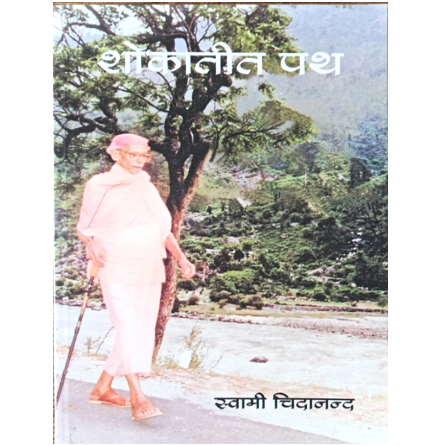
शोकातीत पथ
THE PATH BEYOND SORROW
का हिन्दी अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती
सही रूपान्तरण : श्रीमती गुलशन सचदेव
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय: शिवानन्दनगर-२४९१९२
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dishq.org1010
प्रथम हिन्दी संस्करण : २००८
द्वितीय हिन्दी संस्करण : २०१६
(५०० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
HC 4
PRICE: 140/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए
स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त
फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर-२४९१९२, जिला टिहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड' में मुद्रित।
For online orders and Catalogue visit: disbooks.org
श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती
(जीवन-झाँकी)
श्री स्वामी चिदानन्द अपने पूर्वाश्रम में श्रीधर राव के नाम से ज्ञात थे। उनका जन्म २४ सितम्बर १९१६ को हुआ। उनके पिता का नाम श्रीनिवास राव तथा माता का नाम सरोजिनी था। उनके पिता एक समृद्ध जींदार थे।
स्वामी जी एक मेधावी छात्र थे। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर लेने के पश्चात् सन् १९३६ में उन्होंने लोयोला कालेज में प्रवेश लिया। सन् १९३८ में उन्होंने स्नातक-उपाधि प्राप्त की। इस विद्यालय में ईसाइयत का वातावरण था। इस वातावरण में व्यतीत हुआ उनका अध्ययन-काल उनके लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। हिन्दू- संस्कृति के सर्वोत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट तत्त्वों के साथ समन्वित हो कर प्रभु यीशु, उनके पट्टशिष्यों तथा अन्य ईसाई सन्तों के जीवनादर्शों ने उनके हृदय में स्थान बना लिया। अपने सहज, विशाल दृष्टि-क्षेत्र के कारण वह कृष्ण में ही यीशु का दर्शन (न कि कृष्ण के स्थान पर यीशु का दर्शन) करने लगे। वह जितने विष्णु-भक्त थे, उतने ही यीशु-भक्त भी। कुछ समय तक स्वामी शिवानन्द जी के साथ पत्र-व्यवहार के माध्यम से सम्पर्क रख कर वह सन् १९४३ में आश्रम परिवार में सम्मिलित हो गये।
यह स्वाभाविक था कि अन्तेवासी के रूप में उन्होंने सर्वप्रथम आश्रम के शिवानन्द चैरिटेबल औषधालय का कार्यभार सँभाला। उनके हाथ में रोग-हरण की दिव्य-क्षमता उत्पन्न हो गयी। इस कारण रोगियों की भीड़ बढ़ने लगी।
आश्रम में उनके आने के बाद जल्दी ही उनकी कुशाग्र बुद्धि का पर्याप्त परिचय मिलने लगा। वह भाषण देने लगे, पत्रिकाओं के लिए लेख लिखने लगे तथा दर्शनार्थियों को उपदेशों से लाभान्वित करने लगे। जब सन् १९४८ में योग-वेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय (अब योग-वेदान्त आरण्य विद्यापीठ) की स्थापना हुई, तब पूज्य गुरुदेव ने उन्हें उसके कुलपति तथा राजयोग के प्राचार्य के रूप में नियुक्त करके उन्हें सर्वथोचित सम्मान प्रदान किया। सन् १९४८ में पूज्य स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने उन्हें दिव्य जीवन संघ के महासचिव के रूप में मनोनीत किया। अब संस्था का महान् उत्तरदायित्व उन्होंने अपने कन्धों पर सँभाल लिया।
गुरुपूर्णिमा-दिवस, १० जुलाई १९४७ को पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने उन्हें संन्यास-परम्परा में दीक्षित किया। इसके बाद से वह 'स्वामी चिदानन्द' कहलाये। इस नाम का अर्थ है- जो सर्वोच्च चेतना तथा परमानन्द में संस्थित हो।
गुरुदेव के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका में दिव्य जीवन का सन्देश प्रसारित करने के उद्देश्य से सन् १९५९ के नवम्बर माह में स्वामी चिदानन्द वहाँ की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। मार्च १९६२ में वह वापस लौटे।
अगस्त १९६३ में, पूज्य गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात्, वह दिव्य जीवन संघ के परमाध्यक्ष के रूप में चुने गये। इसके बाद वह दिव्य जीवन संघ के सुविस्तृत कार्यक्षेत्र में ही नहीं, वरन् संसार-भर के अगणित जिज्ञासुओं के हृदयों में भी त्याग, सेवा, प्रेम तथा आध्यात्मिक आदर्शवाद की पताका को ऊँचा उठाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहे।
सन् १९६८ में पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के शिष्यों तथा भक्तों के अनुरोध पर श्री स्वामी चिदानन्द संसार के अनेक देशों की यात्रा करते रहे और प्रारम्भ से ही श्री गुरुदेव के मिशन का कार्य अथक रूप से करते रहे तथा देश-विदेश में दिव्य जीवन का सन्देश पहुँचाते रहे। एक उत्कृष्ट संन्यासी के रूप में आध्यात्मिक चुम्बकत्व के गुण के धनी स्वामी जी अनगिनत व्यक्तियों के प्रियपात्र बन गये तथा संसार-भर में दिव्य जीवन के महान् आदर्शों के पुनरुज्जीवन के लिए सभी दिशाओं में कठिन परिश्रम करते-करते अन्ततः २८ अगस्त २००८ को ब्रह्मलीन हो गये।
प्रकाशकीय
परम पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज द्वारा दिये गये सोलह प्रवचनों के इस सुन्दर संकलन 'THE PATH BEYOND SORROW' का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करते हुए हमें परम हर्ष का अनुभव हो रहा है।
एक प्रकार से ये प्रवचन परम श्रद्धेय श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के सत्संकल्प का परिणाम हैं, जिन्होंने अपने प्रथम शिष्य परम पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज को दिव्य जीवन के जिज्ञासु साधकों तक उनके द्वारा दिया गया सन्देश पहुँचाने के लिए पश्चिम में भेजा।
इन प्रवचनों को दिये गये अनेक वर्ष व्यतीत हो गये हैं; परन्तु इनके अर्थ एवं महत्ता की प्रामाणिकता आज भी उतनी ही है, जितनी कि उस समय थी, जब प्रवचन दिये गये थे। और भी, इन प्रवचनों में दिये गये प्रशिक्षण और पथ-प्रदर्शन के विषय सार्वभौम हैं और इनकी पहुँच अत्यन्त क्रियात्मक है। हमारी हार्दिक आशा है कि यह पुस्तक आध्यात्मिक जीवन के अमूल्य सन्देश को सही रूप में समझने में सहायता करेगी।
- द डिवाइन लाइफ सोसायटी
प्रस्तावना
प्रिय अमर आत्मन् ! शाश्वत ज्योति की दिव्य रश्मियो ! प्रवचनों की इस श्रृंखला में दो शब्द लिखते हुए अतीत प्रसन्नता हो रही है। "भगवान् की शक्ति के रूपों में उपासना के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवचन १९६० में कनाडा में दिये गये थे, जहाँ मैं परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज की ओर से पश्चिम के लिए भारत का योग-वेदान्त सन्देश ले कर उनके (गुरुदेव के) व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में गया था।
गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज सारे भारत में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे। संसार-भर में एक अद्वितीय आध्यात्मिक उद्बोधक और मनुष्य-जाति के मित्र थे, जिन्होंने नैतिक और आदर्श सार्वभौमिक सत्य के प्रसार हेतु अथक प्रचार किया!
पश्चिम में, योग के विषय में अनेक भ्रान्तियाँ हैं। उन्हें वास्तविक योग का ज्ञान नहीं है। अधिकतर लोग कुछ शारीरिक मुद्राओं को ही योग की संज्ञा देते हैं। यद्यपि योग की पुस्तकें अनेक हैं, तथापि योग के आन्तरिक पक्ष का और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की पश्चिमवासियों में महती जिज्ञासा है। व्यक्तिगत अनुभव और गुरुदेव की शिक्षा के आधार पर इन प्रवचनों में मैंने आध्यात्मिक जिज्ञासुओं (विशेषकर पश्चिमवासियों) के समक्ष योग की सत्यता का निरूपण करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि यह छोटा-सा प्रयास योग के प्रति प्रचलित सम्भ्रान्तियों का निराकरण करके इस विषय को उचित रूप से आलोकित करेगा।
योग एक पूर्ण विज्ञान है। सरल भाषा में यदि योग की व्याख्या की जाये, तो जीवात्मा की परमात्मा के लिए स्थिरता ही गति है। दिव्यत्व की ओर स्थिर विकास ही योग है। योग निम्न प्रकृति को दिव्य प्रकृति में परिवर्तित कर देता है। योगाभ्यास से सुस्वास्थ्य, सुख, मानसिक शान्ति और दुःखों से मुक्ति मिलती है।
मानवता एक विशाल परिवार है। विभिन्न जातियों और राष्ट्रों ने मानवता के उद्धार हेतु प्रामाणिक योगदान दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों की सफलता ने अन्ततः मानव मात्र की सफलता के लिए सेवा की है।
योग और वेदान्त से भारत गौरवान्वित है। भारत का आध्यात्मिक आदर्श ही विश्व को एक महान् देन है। योग और वेदान्त अपने क्षेत्र में सार्वभौम हैं। वे समस्त मानव-जाति की सम्पत्ति हैं। आज और आने वाले काल में इन प्राचीन तपस्वियों के ज्ञान से समस्त मानवता प्रेरित हो कर लाभान्वित होगी।
मानवीय कष्टों और समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि सभी राष्ट्र परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करें। रक्तपात और घृणा की अपेक्षा शान्ति और बन्धुत्व भाव से सामंजस्य की स्थिति में मानवीय दशा को चित्रित किया जा सकता है। सृष्टि में ब्रह्म भाव का एकत्व ही जीवन का सार है। आशा करता हूँ कि यह पुस्तक 'शोकातीत पथ' साधकों का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शन करेगी और उन्हें दुःखों से मुक्त करके उन पर सुख-शान्ति की वृष्टि करेगी।
अन्त में, मैं अपने प्रिय मित्र बिल ईलर्स, कैरल शेलडॉन, रोसलिण्ड तथा अन्य मित्रों का उसकी सेवाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद और प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने वाई. एम. सी. ए., वेन्कुवर, बी. सी., कनाडा में मेरे प्रवचनों के लिए सुन्दर प्रबन्ध किया।
'शक्ति देवी के रूप में भगवद्-आराधना' पर प्रवचन डर्बन के विशेषज्ञों के आग्रह पर दिया गया था, जो उस समय अपने समाज में प्रचलित पशुबलि की प्रथा से भयभीत थे।
वेन्कुवर में दिये गये प्रवचन टेप रिकार्ड किये गये और कैरल शैलडन ने ही उन्हें लिपिबद्ध भी किया। इस प्यार भरी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद! श्री स्वामी विमलानन्द और श्री एन. अनन्तनारायणन को भी मेरा हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे कर इस पूर्ण पाण्डुलिपि का निरूपण करके इसे अन्तिम स्वरूप दिया है।
सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का आशीर्वाद उन सब पर रहे, जिन्होंने इस पुस्तक को छपवाने में किसी-न-किसी प्रकार की सहायता की है!
शिवानन्द आश्रम -स्वामी चिदानन्द
२४ सितम्बर १९७५
अनुवादकीय
कोटि-कोटि भक्तों के हृदयों में राज करने वाले शिवानन्द आश्रम के शिरोमणि सन्त श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज आज शरीर से हमारे मध्य नहीं हैं; किन्तु अपने दिव्य ज्ञान की आभा से वे आज भी सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हीं के चरणारविन्द में समर्पित है उनकी अनुपम रचना 'THE PATH BEYOND SORROW' का हिन्दी रूपान्तरण 'शोकातीत पथ' । समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक स्तर के व्यक्ति के लिए इसमें उनके ज्ञान-गर्भित सन्देश हैं। वे लिखते हैं-"मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह उस वस्तु की खोज में दिन-रात संघर्षरत है जो वहाँ है ही नहीं। संसार के अपूर्ण, परिवर्तनशील और अनित्य पदार्थों के मध्य वह सुख की खोज कर रहा है।"
स्वामी जी युवकों के पथप्रदर्शन हेतु लिखते हैं कि बाल्यकाल से ही उन्हें उनके लक्ष्य का बोध कराना प्रत्येक माता-पिता, शिक्षक, वृद्ध का परम कर्तव्य है, अन्यथा युवावस्था में केवल धन अर्जित करना ही मात्र लक्ष्य रह जाता है। सच्चा जीवन जीने की अपेक्षा केवल जीविका-वृत्ति के क्रम में लीन होने के काण उसके जीवन में एक प्रकार की शून्यता का आभास होने लगता है और आन्तरिक सुख का स्थान चिन्ता, अशान्ति और व्याकुलता को मिलता है। सुख एक आन्तरिक दशा है जिसका सम्बन्ध वैभव से कदापि नहीं।
आपके जीवन की व्याकुलता को दूर करने के चार साधन हैं-अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा और सम्मान, समान आयु वालों के साथ मैत्री भाव और बन्धुत्व, अपने से नीच के प्रति करुणा और दया का भाव और दुर्जन के प्रति उपेक्षा का भाव। जीवन में इन चार प्रकार के लोगों से ही आपका सामना होता है। धर्मानुसार जीवन यापन करने वालों का जीवन सुखमय होता है। सर्वोपरि तो यह है कि आप सब सुख, हर्ष और आनन्द के उस महान् आभ्यन्तर स्रोत की सन्निधि प्राप्त करें।
अन्यत्र योग के विषय में कुछ सम्भ्रान्तियों का निराकरण करते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि योग फकीरी नहीं है, शरीर को कष्ट पहुँचाना नहीं है जैसे कीलों पर शयन, भूगर्भ में वास, काँच के टुकड़ों को चबाना, एसिड पीना, सुइयों से शरीर को बंधना इत्यादि । भारत के योगी का यह स्वरूप भी नहीं है कि वह जटाएँ रख कर निर्वस्त्र कीलों की शय्या पर शयन कर रहा है अथवा किसी वृक्ष की शाखा से उल्टा लटका हुआ है। इन सबका योग से कोई सम्बन्ध नहीं है और एक सच्चे योगी को इनसे कोई अभिप्राय भी नहीं है। और भी, योग कोई संस्कार की विधि अथवा अनुष्ठान-विशेष भी नहीं है। भोग-परायणता योग नहीं है। योग प्रतिमा पूजन नहीं है। योग सामुद्रिक विद्या नहीं है। योग भविष्यद्वाद नहीं है। योग कोई विचार अध्ययन नहीं है। योग भूत-प्रेत आदि के निराकरण हेतु मन्त्र-गान नहीं है। योग आपकी दिव्यं प्रकृति के साक्षात्कार का शुद्ध विज्ञान है। योग पूर्णत्व-प्राप्ति का पावन ज्ञान है।
परमात्मा के तेज से प्रकाशित निज आत्मा का बोध करो। भ्रान्तियों के आवरण हटा दो। यही सन्तों का शाश्वत सन्देश है।
सन्तों के जीवन से प्रेरणा लेने का आदेश करते हुए स्वामी जी कहते हैं- "सन्तों की दृष्टि भी सर्वथा अनन्य हुआ करती है। संसारी मानव की दृष्टि 'मैं' और 'मेरा' में रँगी होती है। वह पार्थिव वस्तुओं का आलिंगन करता है। सन्तों के दृष्टि में तो 'मेरा नहीं' का रंग चढ़ा होता है।"
एवंविध, अनेक अमूल्य उपदेशों से अलंकृत इस पुस्तक को पढ़ कर साधकों और सुधी पाठकों को अवश्य ही एक नयी दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
सेविका
गुलशन सचदेव
विषय-सूची
इन्द्रियों का क्षोभ तथा आत्मा का संगीत
आनन्द आपका स्वभाव है : आनन्द आपका पैतृक अधिकार है
धर्म-परायण बनो : सुख-संवर्धन करो
आपकी वास्तविक सत्ता का उच्चतर सुख
२.चमत्कारिक शक्तियाँ और योग में उनका स्थान
विकास-क्रम में योग एक सचेतन त्वरता
शुद्ध चमत्कार की क्रिया योग नहीं
कुण्डलिनी से खेलना अग्नि से खेलना है
गुप्त शक्तियों से सम्पन्न व्यक्ति
चमत्कारिक शक्तियाँ और जिज्ञासु
चमत्कारिक शक्तियों का परित्याग करो
ध्यान का रूप और योग में इसका स्थान
ध्यान की प्रक्रिया प्रारम्भ कैसे की जाये-समुचित विधि
मन को ब्रह्म-विचार से आपूरित करो
आध्यात्मिक आनन्द के विरोधी-विषय-सुख
आधुनिक युग के मिथ्या सिद्धपुरुष
मानव-विश्लेषण की भौतिक उपेक्षा
सार्वभौमिक तत्त्व 'मैं' और 'मैं हूँ'
मिथ्या ऐक्य-भाव सार्वभौमिकता को नष्ट करता है
प्रभु के संग चलो, प्रभु के संग सम्भाषण करो
६. आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य
जीवन के सच्चे उद्देश्य की प्रतीति हेतु समुचित शिक्षण
भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य
आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में समन्वय
७. स्वास्थ्य और समृद्धि के नियम
स्वस्थ रहने के लिए भोजन कैसा हो?
आत्म-संयम और जीवन-शक्ति की रक्षा
शरीर और मन-व्याधि और अधिव्याधि
त्रिदोषों का आयुर्वेदिक सिद्धान्त
समृद्धि का आध्यात्मिक सिद्धान्त
गृह-समृद्धि हेतु कतिपय अमोघ सूत्र
८. शक्ति देवी के रूप में भगवद्-आराधना
स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक जीवन-गाथा
मानव-जीवन के चार प्रमुख स्वरूप
शिशुओं का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शन
गृहस्थी के लिए आध्यात्मिक दिनचर्या
क्रियाशील आध्यात्मिकता-भगवद्-स्मरण
मनुष्य-स्वयं भाग्य-निर्माता है
कर्म का विधान और ईश्वर का न्याय
११. रहस्यमय मन और उसका नियन्त्रण
मानव और ईश्वर के मध्य मन-एक बाधा
पाश्चात्य मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव
सूक्ष्म संस्कारों की प्रक्रिया
राजयौगिक कला में चयनशील विचारधारा
मन को संयत करने की एक विधि-हठयोग
१२. सच्चे सुख का एकमात्र स्रोत
विषय-सम्पन्नता का आशय सुख नहीं
इन्द्रिय-विषयों का सीमित उपयोग
समय की कसौटी पर खरे उतरे-सुख के साधन
शोक, दुःख और पीड़ा-योग की उत्पत्ति
व्यावहारिक अनुभव पर आधारित विज्ञान
भारत के सन्तों का आध्यात्मिक अन्वेषण
शुचिता-सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आधारशिला
ध्यान में शरीर, मन और प्राण की भूमिका
मनःप्रसाद हेतु श्वास-प्रक्रिया
शास्त्रों और मतों के परस्पर विरोधी वचन
सन्तों के जीवन से अमोघ मार्ग-दर्शन
निरभिमानता ही सच्चा साधुत्व है
आध्यात्मिक जिज्ञासु के रूप में महात्मा गान्धी
संक्षेप में दिव्य जीवन के मूल तत्त्व
१. आनन्द अपने भीतर है
प्रिय अमर आत्मन्! मैं इसे अतीव हर्ष का विषय तथा अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि भगवान् ने मुझे इस पार्थिव जगत् में आपके रूप में अभीप्सु, जिज्ञासु आत्माओं की यत्किंचित् सेवा का अद्वितीय अवसर प्रदान किया है। इस विशिष्ट कृपा के लिए मैं उस प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो आप सबकी अन्तर्यामी सत्ता का स्रोत है, सर्वव्यापक सत्ता है, अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है तथा इस क्षण भी हमारे मध्य अदृश्य रूप में विद्यमान है और हमें आनन्दित कर रहा है।
इस पुस्तक का नाम 'शोकातीत पथ' अनायास ही मेरे मन में आया, जब मुझे विभिन्न स्रोतों से उद्धरण की एक लघुकाय पुस्तिका मिली जिसमें मानव की समस्याओं से सम्बन्धित विभिन्न शास्त्रों से उद्धृत छोटी-छोटी लोकोक्तियाँ दी गयी थीं। इस पुस्तक को सहज ही 'भागवत पथ' की संज्ञा दी जा सकती थी; क्योंकि यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सब दुःखों का मूलभूत कारण यह है कि हमने असीम आनन्द के, कभी समाप्त न होने वाले अजस्र स्रोत से अपना शाश्वत सम्बन्ध विस्मृत कर दिया है, जो परमानन्द प्रदायक है और अखिल ब्रह्माण्ड के समग्र सुखों से अतिशय सुखमय है। उस सत्ता से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेने पर यह स्वाभाविक ही है कि हम उस वियोग का अनुभव करें, उस अनुभूति से अपने को वंचित अनुभव करें जो कि उसका स्वरूप है। आनन्द तो शाश्वत सत्ता में, उस महान् सत्य में है जो एकमात्र निर्विकार है, अनन्त है, जो नित्य है, सत् है। उस आनन्द के साथ जीवन-सम्पर्क से वंचित होने के विषाद के रूप में वियोग की अनुभूति होती है। उस सच्चे सुख के एकमात्र स्रोत के हमारे जीवन से सक्रिय रूप में वियुक्त हो जाने के उपरान्त हम सुख की खोज में निरत होते हैं।
जिस दिशा में सुख निश्चित तथा अचूक रूप से उपलब्ध हो सकता है, उसको छोड़ कर अन्य सभी दिशाओं में उसकी खोज करना एक विरोधाभासी स्थिति है।
इन्द्रिय-सुख सुख नहीं
जब हम मानवीय स्तर के जीवन का निरीक्षण करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? प्रत्येक व्यक्ति सच्चे सुख की खोज में निरन्तर प्रयत्नशील है। सुख स्मित (मुस्कान) की खोज है। हमने अपने भीतर उच्छ्वास और विषाद को, शोक और निराशा को छुपा रखा है। क्यों? संसार में सर्वत्र यही क्यों दृष्टिगत है? इस प्रश्न पर विचार किया गया है, अन्वेषण किया गया है और हमें उत्तर प्राप्त हुआ है। विवेक जागृत होने पर हम अनुभव करते हैं कि हमने कुछ अत्यन्त मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। क्योंकि विषयों वश पथ-भ्रष्ट हो कर हम आनन्द-मार्ग से भी च्युत हो गये हैं। आनन्द और इन्द्रिय-सुख में अन्तर है। आनन्द के पथ से भटक कर इन्द्रिय-सुख-रूपी विपथ पर चलते हुए लक्ष्य पर पहुँचने के लिए मानो हम एक वन में भटक गये हैं जहाँ हमें उचित दिशा का और उचित पथ का ज्ञान नहीं रहा।
हम अपना पथ क्यों भूल गये? सब प्राणी वास्तविक सुख की खोज में निरत हैं; किन्तु उस खोज में वे असफल क्यों हैं? कारण यह है कि उनमें से अधिकांश प्रारम्भ ही ठीक प्रकार से नहीं करते। आनन्द की खोज प्रारम्भ करने से पूर्व व्यक्ति को यह ही स्पष्ट नहीं होता कि उस आनन्द की प्रकृति क्या है जिसकी उसे खोज है और उसका अधिवास कहाँ है ? हम लक्ष्य से अनभिज्ञ हैं और हमें यह भी ज्ञान नहीं है कि वास्तव में हमें प्राप्त क्या करना है। अपने लक्ष्य एवं प्राप्य से अनभिज्ञ होते हुए भी हमने यह खोज आरम्भ कर दी है। इसका एकमात्र कारण वह परिवेश है जिसमें हम उत्पन्न हुए हैं। हमने ऐसे संसार में जन्म लिया है जहाँ हमारे परिपार्श्व के सब प्राणी किसी-न-किसी कामनापूर्ति में यत्नशील हैं, विशेष रूप से व्यवहार कर रहे हैं और हम सोचते हैं-"हमने इसी प्रकार के लोगों में जन्म लिया है और हमें भी इसी भाँति व्यवहार करना है।" इस प्रकार रहने का वह ढंग सबके साथ स्वचालित ढंग हो गया है। हमने जीवन की एक विशेष परिस्थिति में जन्म लिया है। अनादि काल से इस धारा में अन्य प्राणी बहे जा रहे हैं। हमने भी उसी में पदार्पण किया है और वह है-निराशा, अश्रु, अज्ञान, शोक और दुःख का भँवर - इस भूतल पर सन्देहावस्था जो अपरिहार्य है। सुख से सत्यानन्द की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती; क्योंकि सुख उस अनुभव का ही नाम है जो इन्द्रिय-विषयों के सान्निध्य से उत्पन्न होता है और स्वाभाविक ही है कि इन्द्रिय-विषयों में निहित दोष का अंश उस सुख में भी आता है।
सब विषय देश और काल की सीमा में प्रतिबद्ध हैं। वे न तो नित्य हैं और न ही पूर्ण। वे दोषपूर्ण, परिवर्तनशील और गमनशील हैं। वे मिश्रित अनुभव प्रदान करते हैं, विशुद्ध नहीं। सब सुख अपूर्ण हैं; क्योंकि वे उन विषयों से उद्भूत हैं जो स्वयं अपूर्ण हैं। ये इन्द्रिय-सुख अत्यन्त सन्दिग्ध प्रकृति के हैं और वे विभिन्न पाक्षिक परिणामों से युक्त हैं। सम्पर्क से उद्भूत प्रत्येक इन्द्रिय-अनुभव के साथ उसकी प्रतिक्रिया भी अवश्यमेव
आनन्द अपने भीतर है सम्बद्ध होती है। यदि आप किसी सुस्वादु पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, जब कि आप उसका स्वाद ही चख रहे हैं, तो भी एक भय-सा आपके मन में होता है कि कल कहीं आपको एक गुटिका (गोली) अथवा औषध न लेनी पड़े। प्रत्येक इन्दिय-अनुभव की एक प्रतिक्रिया होती है जो चिन्ता एवं अशान्ति को जन्म देती है। अन्ततोगत्वा ये इन्द्रिय-सुख पूर्णतया निषेधार्थक अनुभव सिद्ध होते हैं और सुख अथवा आनन्द कहलाने योग्य भी नहीं रहते। वे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हैं।
मनुष्य की त्रिकोणी प्रकृति
मनुष्य की त्रिकोणी प्रकृति का अंशभागिन् प्राणी है। एक बुद्धिमान् प्राणी होने के नाते, साथ ही आपमें एक अंश है जो अपनी अभिव्यक्ति में अनार्य (अधम) है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोगासक्ति और अज्ञान-जैसी अधम प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है। मनुष्य का अपरिहार्य अंग होते हुए भी न्यूनाधिक यह स्थूल विषयात्मक पाशविक वृत्ति पाशविक स्तर में होती है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और कहा जाता है कि मनुष्य में वस्तुतः पशु-वृत्ति और वासनाएँ निहित हैं; किन्तु वह उत्कृष्ट गुण, ज्ञान-शक्ति, विचार, बुद्धिजीवी विचार, उत्कृष्ट एवं विवेकपूर्ण विचार से भी युक्त है, इन्हीं से वह मनुष्य कहलाता है; किन्तु मनुष्य का भौतिक अंश पशु ही है। अपने भीतर आपका सत्य नित्य तत्त्व भी है जिसे पूर्णतया विस्मृत एवं उपेक्षित कर दिया गया है। कदापि उसकी अवेक्षणा नहीं की गयी। आपकी मनोवृत्तियों एवं व्यक्तित्व की अधम, स्थूल पाशविक वृत्तियों से सर्वशः अवगुण्ठित यह विविक्त स्थान (कोने) में आसीन है। यह वही त्रिकोणी प्रकृति है जिससे आप स्वयं में 'अहं' का अनुभव करते हैं।
मानसिक ताप
मस्तिष्क ही वह तत्त्व-विशेष है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुष्य को प्रभु की यह एक सन्दिग्ध देन है। यह मनुष्य के लिए अति-सुखद देन है। यह मनुष्य के लिए अति-सुखद अभिप्राप्ति नहीं है; क्योंकि यद्यपि बुद्धि और विवेक उत्तम हैं, तथापि इनका प्रयोग उस प्रकार नहीं होता, जैसे होना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति तो बुद्धि का प्रयोग करते ही नहीं और जो इसका प्रयोग करते भी हैं, उन मनुष्यों में, जो विषयासक्त हैं, यह बुद्धि इन्द्रिय-सन्तुष्टि के साधन एवं मार्ग खोजने और इन्द्रियों की सभी कामनाओं की पूर्ति के कार्य में सहभागिनी बन जाती है। ज्ञानयुक्त अभ्यास जिसके कर्म का अंश है, ऐसा मानव-मन अनन्त इच्छाओं से संलक्षित है। गहन सुषुप्ति की अवस्था को छोड़ कर (अन्य समय में) मन कदापि शान्त नहीं रहता, क्षण-भर के लिए भी नहीं। मन सदैव कर्मरत एवं ताप की अवस्था में रहता है। आपको इस ताप का ज्ञान भी नहीं होता; क्योंकि मन आपको निरन्तर व्यस्त रखता है। इसका अधिकांश समय तात्कालिक इच्छापूर्ति में संलग्न रहता है, इसलिए आपको इसका ज्ञान नहीं रहता। यदि आप कुछ समय के लिए मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को रोकने का यत्न करें और इसका निरीक्षण करें, तो इसमें निरन्तर गति, अनवरत रोष और इच्छाओं के कारण इसकी व्याकुलता की उग्र प्रकृति प्रत्यक्ष सामने आती है और आपको अपने मन के रहस्य का बोध हो जाता है। इच्छाओं से परिपूर्ण सदैव अस्थिर मन ही अनित्य इन्द्रिय-सुख की बहिर्मुखी खोज का मूल कारण है।
इन्द्रिय-सुख की प्रक्रिया
होता क्या है? मन में इच्छा उत्पन्न होती है जो तृष्णा का रूप धारण कर लेती है और आप तृष्णा की पूर्ति हेतु किसी विषय के पीछे भागने को उत्तेजित हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपको आनन्द मिला है। आप स्वयं से कहते हैं- "आनन्द आ गया। मैंने इन्द्रिय-विषय का सुखास्वाद लिया।" वस्तुतः यह तथाकथित अनुभव जो आपको हुआ है, आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, यह मात्र भ्रम है। आप यदि इसका विश्लेषण करें, तो विदित होगा कि इन्द्रिय-सुखार्थ प्राप्त यह अनुभव वस्तुतः इच्छा की तीव्रता शान्त होने पर मन में उद्भूत क्षणिक शान्ति है। इच्छा उत्पन्न होने पर मन को जब तृष्णा ने वशीभूत कर लिया, तो मन विह्वल हो उठा। उसकी शान्ति, प्रसन्नता, स्थिरता लुप्त हो गयी। जब तक तृष्णा रही, मन अशान्त रहा, उद्विग्न रहा और पदार्थ (विषय) प्राप्त होने पर उसका इन्द्रियों ने उपयोग किया चाहे यह जिह्वा, चक्षु, कर्ण, स्पर्श का हो अथवा घ्राणेन्द्रिय-सुख हो। तृष्णा की सन्तुष्टि होने पर मन की अशान्ति एवं उत्तेजना, जो मूलतः तृष्णा के कारण उत्पन्न हुईं, कुछ समय के लिए प्रशान्त हो जाती हैं। तृष्णापूर्ति के पश्चात् क्षणिक शान्ति मिलने पर आपकी कर्मेन्द्रियाँ आपको विषय द्वारा प्राप्त सुखद अनुभव का श्रेय उस पदार्थ को देती हैं अर्थात् आप सोचते हैं कि उस पदार्थ ने ही आपको सुख प्रदान किया है। सत्य यह है कि यह इन्द्रिय-सुख का अनुभव पदार्थ द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। आपको प्राप्त अनुभव मन की उत्तेजना से मुक्ति प्राप्त होने का नकारात्मक भाव है। एवंविध, जब भी आप मनोद्वेग से मुक्ति पाते हैं और सोचते हैं कि आपको प्रत्यक्ष आनन्द की अनुभूति हुई है, तो यह वस्तुतः वासनाओं की उत्तेजनावश प्रदीप्त अन्तःकरण की अग्नि की शान्ति की नकारात्मक अनुभूति है।
वस्तुतः सच्चा सुख, मन की शान्ति और अनुद्विग्नता में है। शान्त मन भी तब तक हमारे वश में नहीं है, जब तक हम यह न समझ लें कि बाह्य विषय-सम्पर्क से उद्भूत सभी अनुभव नकारात्मक हैं और उनका कोई प्रत्यक्ष मूल्य नहीं है। इन बाह्य अनुभवों के फलस्वरूप हमारे मन को, मानसिक तृष्णा को और उद्वेग को केवल तात्कालिक शान्ति मिलती है। संयोगवश, इन्द्रियों का विषयों से सम्पर्क और तात्कालिक सन्तुष्टि की भावना का निकट-सम्बन्ध होने के कारण हम सोचते हैं कि ये दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं। यथार्थतः मन के पुनः प्रशान्त अवस्था को प्राप्त कर लेने से ही आपको तत्काल सन्तुष्टि का आभास होने लगता है।
कल्पना करें कि हिम-शिशिर दिवस में आप शीत ग्रस्त हो गये हैं, आप शीघ्र ही किसी कक्ष में आ कर अग्नि तापते हैं, कोई गरम पेय पीते हैं, स्वयं को गरम कम्बल से ढक लेते हैं और कहते हैं- "अहा! अब कितना अच्छा लग रहा है।" वास्तव में हुआ क्या है कि शीत का दुःखद अनुभव और आपकी व्याकुलता तीन कारणों से दूर हुई है, वे हैं स्वयं को गरम करना, ढकना और गरम पेय का एक प्याला पीना और आप सोचते हैं कि यह सुख है। किन्तु जो व्यक्ति पूर्वशः ही कक्ष में है और जिसने शीत का नकारात्मक अनुभव नहीं किया है, उसके लिए इन बातों का विशेष मूल्य न होगा, जैसा कि आपके लिए; क्योंकि दुःख से मुक्ति आपके लिए सुख के समान थी। यदि आप बुद्धि से काम लें और मनुष्य को प्राप्त होने वाले प्रत्येक संस्पर्श से उद्भूत सुख का विश्लेषण करें, तो आपको ज्ञात होगा कि वे (सुख) किसी दुःखद अनुभव से मुक्ति मात्र हैं, यद्यपि मनुष्य भ्रमवश उन्हें (उन सुखों को) प्रत्यक्ष मानता है। गरमी लगने पर जल में डुबकी लगाने से आपको विश्रान्ति का आभास होता है अथवा उपाहारगृह में जा कर 'मिल्क शेक' अथवा कोका कोला लेने से सुख का अनुभव होता है; क्योंकि आप अत्यन्त उष्ण स्थान से बाहर आये हैं, जहाँ आप सुखी नहीं थे और कदाचित् आपका प्रस्वेद स्रवण हो रहा था। शीतल पेय लेने पर आप प्रसन्न होते हैं; पर वास्तव में उस काल के लिए आपका उष्णता एवं प्रस्वेद का दुःखद अनुभव दूर हो जाता है। बाह्य पदार्थों के सम्पर्क में प्राप्त प्रत्येक अनुभव इसी प्रकार का होता है। पूर्वगामिन् दुःखद अनुभव से क्षणिक मुक्ति दिलाने के साथ ही इसमें कुछ प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाओं की शक्ति भी निहित है। आप एक सुन्दर रात्रि-भोज में बैठे और आपको सुख मिला। वास्तव में सुख इस कारण मिला कि आप क्षुधार्त थे और भोजन खा कर आपने अपनी क्षुधा को शान्त किया। आप सोचते हैं कि इच्छापूर्ति वस्तुतः मेज पर रखे भोजन के खाने से हुई है, यद्यपि आपको भोजन ने क्षुधा के कारण प्रसन्न किया। अन्य व्यक्ति को, जिसे भूख न हो और भोजन की इच्छा न हो, भोजन प्रसन्न न करता। वह यह कहते हुए उससे मुख मोड़ लेता -"नहीं, धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए।" मेज तक ले जाने वाले क्षुधा-रूपी दुःखद अनुभव के अभाव में उसे कोई प्रसन्नता न होती। वह भी यदि क्षुधार्त होता, तो उसे भी रात्रि-भोज में समान रूप से स्वाद का सुख प्राप्त होता। अतः संसार के सभी सुखों के अनुभव पूर्वगामिन् दुःखद अनुभवों से मुक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं।
इन्द्रिय-जनित सुख की प्रकृति यही है। अवतरण द्वारा भूतल को सुशोभित करने वाले परमात्मा के महान् प्रतिनिधि भगवान् कृष्ण अपने अलौकिक गीत 'गीता' में कहते हैं-"सभी इन्द्रिय-सुख दुःख का कारण हैं। इन्द्रिय-जनित सुखों को छोड़ कर हमारे सुख और क्या है? स्वादु पदार्थ से जिह्वा का सम्पर्क, हस्त का किसी प्रिय वस्तु से संस्पर्श, आँखों को किसी वस्तु का दर्शन, कर्णेन्द्रिय का मधुर श्रुतिमनोहर एवं प्रिय बात का श्रवण और घ्राणेन्द्रिय का सुन्दर सुगन्धित पदार्थ से सम्पर्क-यह हमारे सुखद अनुभव हैं। यदि हमें अप्रिय वस्तुएँ दी जाती हैं, तो तत्काल हम क्षुब्ध हो उठते हैं। इन्द्रियों का प्रिय वस्तु से संयोग, हमारा उसमें मोह उत्पन्न होना और ऐसी वस्तु का त्याग जिसके मोह में हम फंसे हुए हैं, दुःख और विषाद का कारण हैं। कदाचित् ऐसा भी होता है कि जिस पदार्थ ने कभी आपको आकर्षित किया, स्वरूप परिवर्तित होने पर वही आपके दुःख का कारण बन जाता है। अतएव, अप्रिय वस्तु का सम्पर्क दुःख है, प्रिय एवं सुखद वस्तुओं का त्याग दुःख है, और किसी प्रिय वस्तु का स्वभाव परिवर्तित होना भी दुःख है। एवंविध सभी बाह्य पदार्थों के संयोग में दुःख का बीज निहित है। वे अन्तर्हित दुःख के प्रबल स्रोत हैं। उनका आदि है और अन्त भी है। अतः बुद्धिमान् व्यक्ति उनके साथ कभी भी प्रसन्न नहीं रहता। इन बाह्य पदार्थों में वह सुख का अनुभव नहीं करता; क्योंकि उसे इन पदार्थों की प्रकृति एवं तत्त्व का ज्ञान हो गया है। वह कहता है-"नहीं, सभी ऐन्द्रिक अनुभव नकारात्मक हैं। वे प्रत्यक्ष अनुभव कदापि नहीं हैं। वे प्रतिक्रियात्मक भी अवश्य हैं। उनका आदि है और अन्त है।" पदार्थ स्वयं में अपूर्ण हैं; अतः उनसे प्राप्त अनुभूति भी अपूर्ण है; क्योंकि आपको अपूर्ण से पूर्ण की अनुभूति नहीं हो सकती। अतएव विवेकशील मनुष्य इन पदार्थों में सुख का अनुभव नहीं करता।
विवेकशून्य तर्क के दृष्टान्त
बुद्धिमान् कितने हैं? कितने लोग विवेक से काम लेते हैं? हमें विश्व के पदार्थों का विश्लेषण करना है। उनकी वास्तविक प्रकति को देखना है, बाह्य नहीं। केवल विवेकशून्य दृष्टि से उनको देखना नहीं है, वरन् उनकी खोज करनी है। प्रभु से वरदानस्वरूप प्राप्त मेधा को हमें सतर्कता से उपयोग करना चाहिए, पक्षपातपूर्वक नहीं। स्पृहा-युक्त बुद्धि, पूर्वशः ही इन्द्रियों से संयुक्त होने के कारण एवं विषय-वासनाओं की दासी होने के कारण, आपको अयथार्थ निर्णय ही देगी। यह यथार्थ निर्णय कभी नहीं दे सकती। आपकी ज्ञान-शक्ति सत्य एवं शुद्ध होने पर भी यह अत्यन्त 'अविवेकपूर्ण', मिथ्या ज्ञान-शक्ति हो सकती है। यह लोक-विरुद्ध प्रतीत होती है; किन्तु प्राचीन भारतीय पुराणों में ऐसी विनोदपूर्ण कथाएँ लिखित हैं जो बताती हैं कि मनुष्य बुद्धि से काम ले कर भी मूर्खता कर बैठता है। ऐसे ही वह विचित्र मन्दबुद्धि युवा पुरुष की कथा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वह लकड़ी काटने गया और एक वृक्ष की लम्बी शाखा पर चढ़ कर उसे काटने लगा। उसने उसका अवलोकन किया और बोला- "शाखा वृक्ष के मूल की सर्वाधिक स्थूल है और जिस पर मैं बैठा हूँ, वह अपेक्षाकृत पतला है; अतः वृक्ष के मूल की ओर से काटने पर अधिक लकड़ी प्राप्त होगी।" वह अधिक लकड़ी के लालच में पतले भाग की ओर बैठने के लिए मुड़ा। एक पथिक ने उसे पुकार कर कहा- "तुम क्या कर रहे हो ? इस प्रकार शाखा काटना तो मूर्खता है।" किन्तु उसने प्रत्युत्तर दिया - "आपका इसमें कोई मतलब नहीं। मैं जानता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने विचारपूर्वक और सावधानी से यह कार्य प्रारम्भ किया है और इस वृक्ष के हाथों मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता। मैं अधिकाधिक लकड़ी ले जाना चाहता हूँ।" अतः वह शाखा को काटता ही गया और अन्ततः शाखा सहित वह भी नीचे आ गिरा। उस पुरुष ने बुद्धि से काम तो लिया था, अनुमान लगाया और सोचा कि इस विधि से वह अधिक लकड़ी प्राप्त कर सकेगा। वह एक प्रकार से ठीक भी था, किन्तु कदाचित् कोई बात तो थी जो सर्वथा न्यायसंगत नहीं थी। इस कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बुद्धि के विविध रूप हैं।
एक और घटना इस प्रकार है—एक बार एक व्यक्ति को अपनी वृद्ध, जराजन्य मातामही की सेवा का कार्य सौंपा गया। अन्य उष्ण देशों की भाँति भारत में मक्खी और मच्छर अधिक हैं। वह व्यक्ति अपनी मातामही को सतत पंखा किये जा रहा था। यद्यपि वह सोत्साह पंखा कर रहा था, तथापि कुछ मक्खियाँ हट ही नहीं रही थीं। अन्ततः वह बोला- "देखो! मेरी दादी माँ को दुःखी मत करो"; और जोर से निरन्तर पंखा करता रहा। अन्ततोगत्वा वह मक्खियों की दृढ़ता पर अत्यन्त क्रोधित हो उठा और बोला- “देखो, यदि तुम आज्ञा पालन नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें पाठ पढ़ा दूँगा।" तेजी से हवा करते हुए कुछ क्षण के पश्चात् मक्खियों का उतना ही साहस देख कर उसने इधर-उधर देखा और उसे एक दण्ड दिखायी दिया। दण्ड उठा कर वह कहने लगा- "मक्खियों, तुम सोचती हो, तुम मुझसे भी अधिक बुद्धिमान् हो!" ऐसा कहते हुए अवधानपूर्वक उसने दण्ड से एक मक्खी को लक्ष्य बनाया और इस क्रम में वृद्धा दादी माँ का मस्तक फोड़ दिया। हममें से अनेक चतुर तो बहुत बनते हैं; किन्तु मौलिक भूलों से ही कार्यारम्भ करते हैं। उस व्यक्ति के लिए यह ज्ञान अवश्यम्भावी था कि उसकी दादी माँ का जीवन अधिक मूल्यवान् था अथवा मक्खी का। किन्तु वह अज्ञानी था और हम उसका उपहास करते हैं। साथ ही निर्णय लेने में हम स्वयं वही भूल कर बैठते हैं।
इन्द्रियों का क्षोभ तथा आत्मा का संगीत
सच्चे सुख की अनुभूति हेतु मानसिक शान्ति पूर्वाकांक्षित है। क्या वह स्तोक अशान्ति और अभिलाषा, उत्तेजना और कामना की मुक्ति से महत्तर नहीं है? महत्तर क्या है? आप कहेंगे-"इच्छा उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ति ही उससे मुक्ति एवं सुखानुभूति का साधन है।" ऐसा कहते हुए आप इच्छा-रूपी मक्षिका को उड़ा तो देते हैं; किन्तु सच्ची मानसिक शान्ति-रूपी दादी माँ की रक्षा नहीं करते जिसके द्वारा आपको सुख प्राप्त हो सकता है। शान्ति में ही वास्तविक सुख निहित है। स्थिर एवं प्रसन्नचित्त होने पर आपके अन्तःकरण से ही शान्ति और आनन्द का स्रोत फूट पड़ता है। आपको सुख का निर्माण नहीं करना पड़ता; क्योंकि इसका निवास आपके भीतर ही है। परिवर्तनशील, नश्वर भौतिक पदार्थों में सुख नहीं है। सुख यहीं है, जहाँ आप बैठे हैं। आप स्वयं आनन्दस्वरूप हैं। आनन्द आपकी शाश्वत प्रकृति है। इन्द्रियों एवं मनोकामनाओं की प्रकृति से सर्वथा भिन्न आपके व्यक्तित्व का यथार्थ रूप ऊपर है। वही आनन्द है, शुद्ध परम आनन्द! आप क्या है? यदि आप इसकी व्याख्या पूछें, तो मैं कहूँगा - "आप शुद्ध स्वरूप हैं, दोष-रहित हैं, परम आनन्द हैं।" यही आत्मा का लक्षण है। आत्मा आनन्द है, हर्षोन्माद है, विलक्षण आनन्द है। जैसे यह मेज लकड़ी से बनी है, आपके वस्त्र ऊन अथवा सूत से बने हैं, मिश्री शर्करा से बनी है, वैसे ही आपके चैतन्य के मध्य विराजित वास्तविक स्वरूप का तत्त्व और धागा 'अहं' आनन्द से विरचित है। आप आत्म-स्वरूप हैं। आप आत्म-तत्त्व हैं। उल्लास और आनन्द के शाश्वत, नित्य, अविरत, आत्म-स्थित स्रोत हैं। आप यह शरीर, मन और बुद्धि नहीं है।
जीव के प्रति पूर्व और पश्चिम की विचारधारा सर्वथा विरोधी है। पाश्चात्य देशों का कथन है-"मनुष्य बुद्धि-रूपी विशेष शक्ति से युक्त एक पशु है।" हम पूर्ववासियों की धारणा है- "मनुष्य गौरवशाली, सदापूर्ण, अलौकिक, ज्योतिर्मयी, आनन्दमयी सत्ता है; किन्तु बुद्धि अथवा मन-रूपी शक्तियों से युक्त है जो उसके दास हैं और साधन मात्र हैं।" परमात्मा की देन 'मन' ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आप आनन्द, सौन्दर्य, आत्मा की पूर्णता, प्रकटीकरण, अनावरण एवं साक्षात्कार इसी संसार में कर सकते हैं; किन्तु आपने अपने जीवन को संघर्ष बना दिया है। सामान्य व्यक्ति वैश्य का-सा जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी दिव्य प्रकृति को भुला कर उसकी उपेक्षा करने लगा है।
अपनी पशु-वृत्ति को सन्तुष्ट करने में ही वह सम्पूर्ण शक्ति का ह्रास कर देता है। अन्तःकरण में स्थित पशु की वासनाओं की सन्तुष्टि हेतु सतत संघर्ष ही उसके जीवन की एक व्यवस्था बन चुकी है। सुन्दर वस्तुओं का समीकरण, सुन्दर पोशाक, सुन्दर दृश्य और सुन्दर पदार्थों का भोग ही उसका लक्ष्य बन चुका है। सुख, सुख, सुख, सुख की कथित दौड़ में आनन्द का तो मानो विलोप ही हो गया है। इन्द्रिय-क्षोभ के कारण ही कोलाहल इतना हो गया है कि आत्म-संगीत का तो पूर्ण रूप से मानो हनन होता जा रहा है।
मेरे सन्देश में हर्ष का विषय यह है कि इस आनन्द का लोप नहीं हो सकता। यह अविनाशी है। जो आनन्दरूप आप हैं वह भी अक्षय है, अजर है, अमर है, कोई उसका स्पर्श नहीं कर सकता। हृदय के अन्तरंग में जहाँ आप सच्चे आनन्द के रूप में अवस्थित हैं और चैतन्य के अन्तरस्थ कक्ष में, जहाँ 'आत्मा' का वास है, उस उच्छ्रित आत्मिक-राज्य में शोक प्रवेश भी नहीं कर सकता।
आनन्द आपका स्वभाव है : आनन्द आपका पैतृक अधिकार है
नाम और रूप, अमुक श्री एवं श्रीमती जिनसे आपको सम्बोधित किया जाता है, यह 'आप' वास्तविक नहीं है। आपके माता-पिता द्वारा आपके वास्तविक अस्तित्त्व पर यह केवल आरोपित व्यक्तित्व है। उन्होंने आपका नाम रखा है। वे आपको किसी भी नाम से सम्बोधित करें; किन्तु वह नाम-रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। शैशव से यौवन, यौवन से प्रौढ़ावस्था और मध्यावस्था और फिर वृद्धावस्था में सदा एक रूप वही 'आत्मा' है जो आपके अन्तःकरण में विद्यमान है। आपके शैशव में यह आपके भीतर था। बालक बन कर जब आप इतस्ततः दौड़ रहे थे, तब भी यह आपके भीतर था। किशोरावस्था में भी यह आपके अन्तःकरण में था। प्रौढ़ावस्था में सुख के पदार्थों के पीछे भागते हुए जब आप मनसा अशान्त हो गये, तब भी यह आपके भीतर था। गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व से जब आप दबे हुए थे, तभी भी यह आपके भीतर था और वृद्धावस्था पर्यन्त अन्तःस्थित रहेगा।
इस अविकारी आत्मा का बोध करने का प्रयास करें। अन्तर्मुख हो कर मन को संयमित करें। मन को विषयों के प्रति बहिर्मुखी न होने दें। तदोपरान्त अन्तरावलोकन करें और एकान्त में शान्ति से आत्म-विश्लेषण करने का यत्न करें। आप देखेंगे कि शान्ति, आनन्द, सर्वशक्तिमान् और सम्पूर्ण 'अहं' आपके भीतर है। वहाँ कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। वह सर्वसम्पूर्ण है। उस पावन प्रदेश में कोई इच्छा प्रविष्ट नहीं होती; क्योंकि यह अनुभव ही सम्पूर्ण रूप है। आपमें से प्रत्येक व्यक्ति इस सम्पूर्णता, सर्वानन्द और शान्ति का अद्वितीय अनुभव इसी क्षण इसी स्थान पर ले सकता है। इसका निर्माण करना आवश्यक नहीं। उस आनन्दमयी अवस्था की प्राप्ति हेतु आपको अपने से बाहर कहीं नहीं जाना है। यह आपका जन्म-सिद्ध अधिकार है। यह आपका स्वाधिकार है, विशेषाधिकार है जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। इन्द्रियों के दास मत बनो। अपूर्ण लघु पदार्थों के पीछे बाहर भागना त्याग दो। मौन व्रत धारण करो और स्मरण रखो कि आप आनन्द हो, पूर्णत्व से युक्त हो। कामनाओं से ऊपर उठो और अपनी वास्तविक प्रकृति के प्रति जागरूक रहो जो अनुपमेय आनन्द है, अनिर्वाच्य आनन्द है।
मनुष्य होने के नाते से ही इस अनुपमेय आनन्द को प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यह आपका अधिकार है। आदि काल से ही यह आपका पैतृक अधिकार है। आप सबका प्रभव 'आनन्द' के उस अनवरत स्रोत से है जिसे मनुष्यगण 'परमात्मा', 'ऋत', 'सत्य', 'ब्रह्म' आदि की उपाधि से सम्बोधित करते हैं। आप किसी भी संज्ञा से उसका आह्वान करें, किसी भी साधन द्वारा उस तक पहुँचें, स्वेच्छा से मनोनीत अर्चना करें, इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। किन्तु यह ज्ञान करना अनिवार्य है कि आनन्द और सुख का अवर्णनीय, अवाच्य, अनवरत स्रोत इसी स्थान पर आपके अन्तःकरण से शोभायमान हो रहा है। इसकी प्राप्ति हेतु आपकी ओर से क्षुद्र, असार वस्तुओं का त्याग करना तथा उस अनुपम, अप्रतिम, अन्तस्थ शाश्वत शक्ति के लिए तीव्र आकांक्षा और उससे प्रीति के अतिरिक्त आपसे अन्यद् किंचिदपि अपेक्षित नहीं है।
पहला नियम यह है कि अपनी बुद्धि का उपयोग करें और इन्द्रियों के आकर्षक विषयों के भ्रम में न पड़ें। वे आपको गोलाकार चक्र की ओर ले जायेंगे। आपको सुविदित ही है कि तृष्णापूर्ति करते रहने से सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होती। इन्द्रिय-सुखास्वाद तो इच्छापूर्ति नहीं, प्रत्युत इच्छाओं का संवर्धन करता है। एवंविध लालसा कभी समाप्त नहीं होती। आस्वादन तृष्णा को और प्रबल बनाता है। अतः आप इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते। दमन तो आप विवेक की जागृति एवं विषयों के यथार्थ बोध द्वारा यह कहते हुए कर सकते हैं- "दैव योनि के अध्यात्म-रूप के मैं उन तुच्छ पदार्थों की लालसा की अवहेलना करूँगा जो श्वान के समक्ष प्रक्षिप्त अस्थियों के समान है। मैं सम्राटों के सम्राट् की सन्तान हूँ, अमूल्य स्वाधिकार की ही प्राप्ति हेतु प्रयत्न करूँगा, तुच्छ पदार्थों के पीछे नहीं जाऊँगा।" आप यदि ऐसा करते हैं और विवेक से तुच्छ पदार्थों की अवज्ञा करते हैं, तो आप परम ज्योति के उत्तराधिकारी बन जाते हैं।
आन्तरिक वैराग्य द्वारा प्रतीति होती है कि वास्तविक आनन्द क्या है और केवल मिथ्या क्या है और जिस आनन्द की प्रकृति नित्य नहीं है, उसका उत्सर्ग करके व्यक्ति मनसा पराङ्मुखी हो जाता है। विवेक से उद्भूत मानसिक वैराग्य इस आध्यात्मिक जिज्ञासा का रहस्य है। 'शोकातीत पथ' का यह प्रारम्भिक चरण है। एक उपनिषद् में उपदेश है-"हे मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष दो पथ हैं- एक तो केवल आकर्षक और प्रिय है तथा दूसरा जो शुभ और आत्यन्तिक कल्याणकारी है।" अल्पबुद्धि मनुष्य तो प्रिय-प्रेय मार्ग को ही अपनाता है और इस प्रकार वह अपने कल्याण का, श्रेय का विनाश कर बैठता है। विचारशील मनुष्य विवेक के जागृत होने पर दोनों मार्गों का परीक्षण करता है और आकर्षक तथा प्रिय मार्ग की सत्य प्रकृति को जान लेता है और उसकी उपेक्षा करते हुए सर्वदा आनन्द और कल्याणप्रद पथ का अनुगमन करता है। वहाँ उसे वास्तविक आनन्द की प्राप्ति होती है। जीवन में प्रारम्भ से ही सदा, प्रतिदिन आपके समक्ष भी पथ-चयन का अवसर आता है। यह आप पर ही निर्भर है कि आप कौन-सा पथ स्वीकार करते हैं। आप बाह्यतः आकर्षक इन्द्रिय-जनित सुख के प्रलोभन में आ जाते हैं अथवा आपके भीतर विवेक रूपी ज्योति है जो आपको अनिवार्यतः श्रेय पथ की ओर अग्रसर करती है जिसमें आपके जीवन का कल्याण निहित है।
अपना दुःख-अपनी सृष्टि
आपका दुःख आपकी अपनी ही रचना है। यह आत्म-सृष्ट है। इसका कारण अज्ञान और इन्द्रियों की दासता है। स्वयं कारण-रूप होने के कारण अपनी शक्ति द्वारा ही आप इसका निराकरण कर सकते हैं। एवंविध जिस प्रकार आपका दुःख स्व-रचित है, उसी प्रकार आपका सुख भी प्रयत्न द्वारा आपकी अपनी उपलब्धि बन सकता है। है, उके द्वारा इसकी रचना की आवश्यकता नहीं; क्योंकि यह पहले से ही वहाँ पर विद्यमान है। आपने केवल इसे ग्रहण करना है और यह आपके वश की ही बात है। 'वह' तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी अनुभूति हेतु आपको स्वयं ही पग आगे बढ़ाना है।
धर्म-परायण बनो : सुख-संवर्धन करो
इसका सन्निवेश आप कैसे कर सकते हैं? मूल आनन्द धर्म-परायण जीवन से ही प्रस्फुटित होता है। यह मौलिक तथ्य है। योग का यही कथन है। धर्म के बिना आनन्द की प्राप्ति कभी सम्भव नहीं है। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं धर्मोपदेश नहीं कर रहा। मुझे किसी ने कहा- "पाश्चात्य जन-मानस की धर्म में रुचि नहीं है, धर्मोपदेश मत करो।"अस्तु! मैं वह इच्छा तो पूर्ण कर नहीं सकता। आपके समक्ष उपस्थित, आपसे वार्ता करता हुआ यह विनीत सेवक धर्मोपदेश तो करता है; किन्तु वह धर्मोपदेश अन्य प्रकार का है। वह स्वभाव से उपदेश देने का अभ्यासी नहीं, प्रत्युत आपसे भी अधिक विनीत व्यक्ति है जिसे प्रसार का आदेश प्राप्त हुआ है और आपके सेवक के रूप में उसे वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। मैं धर्मोपदेश करूँ तो भी यह तो नहीं कहता कि आप सब अधर्मी हैं और भ्रष्ट देश में पहुँच गये हैं। मैं तो कहूँगा- "अपनी गरिमा का अवलोकन कीजिए जो पूर्वशः ही आपके अधिकार में है। आप इस पर स्वाधिकार क्यों नहीं करते?" मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि आप अत्यन्त अद्भुत वस्तु को खो रहे हैं। इसका विक्षेप मत कीजिए। यही समय है। मनुष्य-जीवन के रूप में उस अलौकिक और महत्तम वस्तु की उपलब्धि हेतु आपको यह अद्वितीय अवसर प्राप्त हुआ है। विलम्ब न करें। आप अपने बन्धन को कामनाओं के कारण बढ़ाना क्यों चाहते हैं? अपनी मुख्य प्रकृति पर अनुशासन की डोर बाँध कर गौरव को क्यों नहीं प्राप्त करते जो आपमें पहले से ही विद्यमान है।
इसे मैं धर्मोपदेश नहीं कहता। मैं आपको एक महत् नियम से केवल यह कह कर परिचित कराता हूँ कि आनन्द की प्राप्ति हेतु धर्म अवश्यम्भावी है। यह केवल मनोवैज्ञानिक नियम नहीं है, प्रत्युत् आध्यात्मिक नियम भी है; क्योंकि धर्म से आपकी प्रकृति शुद्ध होती है। आपकी प्रकृति तीन स्तरों में अभिव्यक्त होती है, वे हैं-शारीरिक स्तर, आन्तरिक स्तर जिसका आपको ज्ञान नहीं है (अन्तरंग में मनः शक्ति का एक स्तर है जो इस शरीर को कर्मण्य और स्फूर्तिदायक बनाता है) और आपके मन का तृतीय स्तर जहाँ विचार, तर्क और इच्छाएँ निरन्तर कार्यरत रहती हैं। धर्म आपके जीवन का वह शक्तिपूर्ण तत्त्व है जो आपके व्यक्तित्व की त्रिगुणी प्रकृति को सर्वथा परिष्कृत कर देता है। यह शरीर, मन और बुद्धि को परिष्कृत करता है। शुद्ध और पवित्र मन में ही स्थिरता, सन्तुलन और इच्छाओं का अभाव सम्भव है।
कठोर परिश्रम करने पर भी अपवित्र मन से इच्छाओं का निराकरण सरल नहीं; क्योंकि मानसिक अशुद्धता और इच्छा समानार्थक हैं। उपर्युक्त तीनों स्तरों पर राग और अशुद्धि आपके सम्पूर्ण अस्तित्त्व को उद्वेग की अवस्था में डाल देते हैं। राग की प्रकृति में उद्वेग छिपा हुआ है। इस प्रकार दृढ़ता, अवस्थिति, शक्तिमत्ता और अन्तर्मुखता पवित्रता का स्वभाव ही है। अतएव यह गहन आध्यात्मिक सत्य है कि शुद्धि, सरलता, सत्य, करुणा, निःस्वार्थता और नम्रता आदि सद्गुणों का समावेश और लोभ, मोह, ईर्ष्या-द्वेष आदि भावों का निराकरण आपके स्वभाव को शनैः शनैः परिवर्तित करके इसे परिष्कृत, पवित्र और सूक्ष्म बनाता है। पवित्रता के आने पर मन की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। आतुरता से इन्द्रिय विषयों की ओर भागने वाला मन अन्तर्मुख हो कर प्रशान्तावस्था में पहुँचने लगता है। मैं 'अन्तर्मुखी' शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। वास्तव में मन अन्तःस्थित हो जाता है, इसकी बहिर्मुखी प्रवृत्ति शान्त हो जाती है। इस प्रकार शुद्धि से संहरण द्वारा आपको आत्म-जनित आनन्द की झलक मिलने लगती है। यह प्राचीन व्यंजन है; किन्तु यही प्रवाहशाली है। अपवित्र रह कर कोरे आनन्द की आशा नहीं की जा सकती।
अज्ञानान्धकारवश भोग विलासों में आसक्त व्यक्ति सुख नहीं पा सकता। स्वार्थपरक एवं कठोर बन कर आप दूसरों को कष्ट दे कर दुःखी करें और साथ ही सुख प्राप्ति की अभिलाषा रखें, तो यह असम्भव है। दूसरों को आप जितना अधिक सुख पहुँचायेंगे, आप स्वयं उतना अधिक सुख का अनुभव करेंगे। यह विधान है। अपनी प्रकृति की परिष्कृति, संस्कृति और सम्पूर्ण व्यक्तित्व की पवित्रता-जीवन में आनन्द के उदय हेतु अवश्यम्भावी रूपेण पूर्वापेक्षित है। इस प्रकार दैनिक जीवन में सोत्साह धर्म के अभ्यास, बहिर्वृत्ति-निग्रह और स्वार्थभाव से आनन्द आविर्भूत होता है। यह शाश्वत नियम है और मानव की सत्ता के अस्तित्त्व पर्यन्त मानव में कार्यशील बना रहेगा। यही प्रभाविक युक्ति है। आपके पवित्र होने पर अपवित्रता से आने वाले सब दोष दूर हो जाते हैं। आप यदि सरल स्वभाव हैं, तो इच्छा-ग्रस्त व्यक्तित्व से उत्पन्न होने वाले विघ्न और क्षोभ समाप्त हो जाते हैं। सादा जीवन आपको अनवरत इच्छाओं के बोझ से मुक्त करता है। यदि आप सत्यशील हैं, तो आपको स्वयं ही ज्ञान हो जायेगा कि निरन्तर भय और चिन्ता से ग्रस्त असत्यवादी विश्व अचिरेण ही विलीन हो जाता है। एक झूठ को छिपाने के लिए आपको दर्जनों झूठ बोलने पड़ते हैं और इससे आपका मन सतत भयभीत और चिन्तित रहने लगता है- "खोज की जाये, तो परिणाम क्या होगा?" सत्यनिष्ठ होने पर भय, चिन्ता और असत्य से उत्पन्न क्षोभ से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है।
सन्तोष! आप जब सन्तुष्ट हैं तो आप अखिल विश्व के सबसे धनी मनुष्य हैं। आपको कोई ईर्ष्या नहीं है। आप अपनी सम्पन्नता से सन्तुष्ट हैं। आपको अपने से अधिक समृद्ध व्यक्ति के साथ द्वेष नहीं है, प्रत्युत आप पर-समृद्धि में प्रसन्न हैं।
आपकी वास्तविक सत्ता का उच्चतर सुख
निम्न मनोवैज्ञानिक स्तर पर सुख का अनुभव प्राप्त करने के लिए आनन्दानुभूति हेतु गुण-वृद्धि सहज साधन है; किन्तु उच्चतर स्तर पर यह पर्याप्त नहीं है। यद्यपि मानसिक स्तर पर प्राप्त आनन्द भी आपको अत्यन्त हर्षप्रद प्रतीत होगा, तथापि इसमें ही आपको सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए। यह भी एक महान् प्राप्ति है; किन्तु आपका लक्ष्य आनन्द-प्राप्ति ही होना चाहिए जो इससे भी बढ़ कर है। वह उच्चतर (परम) आनन्द आपके वास्तविक अस्तित्त्व, आपकी वास्तविक प्रकृति, अन्तरात्मा और शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से परे का आनन्द है। इन सबसे उदात्त है-शाश्वत, अविकारी, मौन चैतन्य जो आपकी सत्ता के निम्न पक्षों की विकारी वृत्तियों से ऊपर है। आप मन नहीं हैं; मन आपका साधन है। आप देह और इन्द्रियाँ नहीं हैं; देह और इन्द्रियाँ तो आपके बाह्य परिधान हैं। वे केवल आवरण मात्र हैं; आपका भौतिक आवरण हैं। इन सबसे अधिक महान् आपका अन्तःकरण, आपका शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्तित्व है जो स्वयं दिव्यता है। असीम आनन्द इसकी प्रकृति है। दुःख, भय, इच्छा कदापि इसके समीप नहीं आ सकते। अतः प्रतिदिन मौन, एकान्त, अन्तर्मुखी ध्यान में जाने का प्रयास करें। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करें। उस अनुभव का आनन्द तथा उस ज्योति के ईषद्-दर्शन प्राप्त करने पर आप ध्यान कभी न छोड़ेंगे। आप खाना-पीना त्याग सकते हैं; परन्तु एकान्तवास, अन्तर्मुख हो कर अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करने के अवसर का त्याग नहीं कर सकते।
आपके अन्तःकरण में ही 'शोकातीत पथ', शाश्वत सुख का पथ और वस्तुतः सच्चे अर्थों में वास्तविक सुख का पथ निहित है। यह एक दोष रहित सुख का अनुभव है जो किसी भी प्रकार की दुःखद प्रतिक्रिया, अपूर्णता और पार्थिव दोष के लक्षण से सर्वथा रहित है। प्रशान्त, अनिर्वाच्य, ज्योति एवं आन्तरिक सन्तुष्टि से परिपूर्ण यह सुख की परमावस्था है। आप सबमें इस 'शोकातीत पथ' को पार करने की शक्ति निहित है। इसके लिए विशेष योग्यता अपेक्षित नहीं है। आवश्यक नहीं कि आप अभिजात हों, आपके पास बैंक बैलेंस हो, आप एम. ए. पास हों अथवा आपके पास पी-एच.डी. की डिग्री हो। मनुष्य-जीवन दे कर भगवान् ने आन्तरिक अभ्यास करने और इस अद्भुत वास्तविक आनन्द की प्राप्ति हेतु सभी साधन प्रदान किये हैं। तदर्थ आपको अपने आदर्श जीवन की खोज के लक्ष्य एवं परम जिज्ञासा के रूप में उत्तम को ग्रहण करना और अधम का परित्याग करना है। इसे अपना ध्येय बनायें। हृदय में ही सच्चे ईश्वर का साक्षात्कार करें। यही आपके जीवन का प्रमुख ध्येय है। इसके समक्ष अन्य सभी कार्य गौण होने चाहिए। अभीप्सा का प्रधान रूप यही होना चाहिए। इसका अभ्यास करते ही आपको ज्योतिर्मय आनन्द का आलोक प्राप्त होने लगेगा। विवेक द्वारा आपको यह अन्तर्मुखी अभीप्सा जागृत करनी होगी। विषयों की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान करना होगा। अधम तत्त्व का मनसा परित्याग, स्वयं में गहन विश्वास, इस अनुभव की ओर अग्रसर होने के लिए आत्म-शक्ति का विकास एवं इस मुमुक्षुत्व तथा आदर्श प्राप्ति हेतु प्रगाढ़ लगन तथा चिन्तन, मनन, ध्यान के दैनिक अभ्यास का प्रयास करना होगा। यह सर्वोत्कृष्ट सर्वरोगघ्न औषध (त्रिलोक में चिन्तामणि) है। इहलोक और परलोक दोनों के लिए यह सर्वोत्कृष्ट रोगनाशक औषधि है। यह सब दुःख-कष्ट-निवारक है। इसके द्वारा आपको यहीं और अभी अद्वितीयानुभूति होगी, मृत्यूपरान्त किसी अन्य प्रदेश में नहीं। इसी जीवन में इसी क्षण यह अनुभूति होनी चाहिए, ताकि आवागमन के बन्धन से मुक्ति के समय आनन्द से झूमते हुए आप गरिमामय विजयी स्वामी के रूप में विदा हों। वही आपका प्रारब्ध होना चाहिए। आपके जीवन का महानतम लक्ष्य यही होना चाहिए। मृत्यु से भय न हो। किसी प्रकार का भय न हो। आप तो स्वभाव से ही अमर हैं।
हमें केवल उन्हीं पदार्थों का त्याग करना है जो हमारे आनन्द में बाधक हैं। इन लघु ऐन्द्रिक सुखों और पदार्थों की उपेक्षा करने पर हम वस्तुतः त्याग तो कुछ भी नहीं करते, प्रत्युत् ऐसा करना तो बुद्धिमत्ता का कार्य है; क्योंकि हमने उन्हें अपने सुख को चुराने वाले तत्त्व के रूप में जान लिया है। वे अमूल्य वस्तुओं का नहीं, प्रत्युत् अपने परम सुख के शत्रु का त्याग करते हैं जो सुख के अनुभव में विघ्न रूप बन कर समक्ष आते हैं। एवंविध हम उन तत्त्वों का निराकरण करते हैं जो किसी ऐन्द्रिक अनुभव की प्रकृति में मिथ्या आवरण द्वारा वास्तविक सुख का नाश करते हैं जो कदापि सत्य नहीं हैं और कदापि प्रत्यक्ष नहीं हैं।
अतएव अपने जीवन को प्रज्ञा, सामान्य ज्ञान और तात्त्विक सत्य के स्तम्भ पर खड़ा करें। सत्य और विवेकपूर्ण ढंग से बुद्धि का प्रयोग करें और मत भूलें कि बाह्य पदार्थ परानुभूति नहीं करा सकते। विवेकी बनें और सदा खोज करते रहें कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, नश्वर क्या है और अनश्वर क्या है, अधम, परिवर्तनशील और क्षणिक क्या है तथा उत्तम, अविकारी और शाश्वत क्या है! इस प्रकार विवेकशील हो कर शाश्वत की ओर बढ़ें, जो पूर्ण है, चिरस्थायी है, वास्तविक है। इसके विपरीत स्वभाव के सभी पदार्थों का परित्याग करें। यही प्रवीर (Heroic) जीवन है।
आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे! अन्तःस्थित शाश्वत परमात्मा आप पर अपनी दिव्य कृपा की वृष्टि करें ! भूत एवं वर्तमान के, पूर्व और पश्चिम के महान् ऋषि-मुनि आपको आशीष दें और परमानन्द, परम ज्योति के पथ की ओर गमन के लिए प्रेरणा और शक्ति दें तथा इसी समय यहीं इसी जीवन में आपको इस परम आनन्द से परिपूर्ण करें!
परम आत्मिक अनुभूति, सात्यिक अनुभूति एवं आन्तरिक आनन्द के साक्षात्कार के पुरोगम 'शोकातीत पथ' पर अग्रसर, इस अत्यन्त विनीत सेवक, सहगामी बन्धु की यही सकामना है और हार्दिक प्रार्थना है। भगवान् आप सबको आशीर्वाद दें!
२.चमत्कारिक शक्तियाँ और योग में उनका स्थान
'योग' शब्द दुर्भाग्यवश असामान्य आश्चर्यपूर्ण अनुभवों, रहस्यपूर्ण घटनाओं तथा गुप्त चमत्कारिक शक्तियों से सम्बद्ध माना जाता है। प्रायः 'योगी' शब्द का अर्थ 'योग' में कुशल नहीं, वरंच कुछ विशेष चमत्कार दिखाने वाला असाधारण व्यक्ति माना जाता है। कदाचित् यह सत्य भी है; क्योंकि योगी में वह कार्यक्षमता निहित है जो अन्य जनों में असम्भव है; किन्तु योगी की अवधारणा केवल वायु में उड़ने में समर्थ, मासों पर्यन्त निराहार रहने, सप्ताहों पर्यन्त भूमि में दबे रहने अथवा इसी प्रकार के अन्य असामान्य कौतुक दिखाने में समर्थ होने में ही नहीं होनी चाहिए- जो दृष्टिगत न होने पर अविश्वसनीय प्रतीत हो।
ये मिथ्यावाद अधिकांशतः दूरी के कारण उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि दूरस्थ प्रत्येक वस्तु प्रायः रहस्यपूर्ण प्रतीत होती है। इसका कारण वे हास्यप्रद कथाएँ भी हो सकती हैं जिनका इन कौतुकों के कारण प्रचार किया गया है।
योगी शब्द की प्रचलित अवधारणा अत्यन्त मिथ्या और अयथार्थ होने पर भी पूर्ण रूप से निराधार नहीं है, प्रत्युत् उस आधार को अत्युक्ति, विचेष्टित एवं विस्तृत करके सन्दर्भ से दूर कर दिया गया है। उसे ऐसा मोड़ दे दिया गया है जिससे उसका यथार्थ रूप सर्वथा छिप गया है।
योग में आलोक तत्त्व है और निस्सन्देह अनुभव के रहस्यपूर्ण तत्त्व भी हैं; परन्तु ये वे नहीं जो बना लिये गये हैं। इन आलोकों का आधार क्या है; और इनकी व्याख्या क्या है? इनके प्रति विद्वानों का मत क्या है? ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर विचार रोचक ही नहीं महत्त्वपूर्ण भी है; क्योंकि आप सब साधक हैं और इसका एक पक्ष तो कुछ-कुछ आपके अपने ही व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है।
आज के प्रवचन का विषय अलौकिक तत्त्व ही नहीं प्रत्युत् 'योग में अलौकिक तत्त्व' है। कहा गया है कि 'अलौकिक तत्त्व' का अर्थ कोई भी रहस्यमयी वस्तु है-अगोचर, रहस्यपूर्ण अथवा गुप्त। आज हम योग के पथ पर अग्रसर शिक्षकों एवं साधकों के अभ्यास में घटने वाली इन क्रियाओं से सम्बद्ध विषय पर विचार करेंगे। अतः हम इस रहस्यमय तत्त्व को योग-पद्धति के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे।
विकास-क्रम में योग एक सचेतन त्वरता
सर्वप्रथम, जीवन में यौगिक क्रम के प्रति सुस्पष्ट अवधारणा आवश्यक है। प्राणी मात्र का लक्ष्य विकास है और हम सब आत्यन्तिक पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं; क्योंकि एक बार पुनः हमें उस स्वाभाविक दिव्यता का साक्षात्कार करना है। कदाचित् मानव-विकास के सामान्य क्रम की गति अत्यन्त ही धीमी है, कदाचित् असंख्य वर्षों और जन्मों तक इसका विस्तार होता रहे यदि हम प्रत्येक जन्म में कतिपय उन्नत पग उठाते रहें। प्रत्येक जन्म में कतिपय उन्नत पग उठाने के क्रम में दैहिक बन्धन एवं इच्छा-अनिच्छा, राग और वैराग्य की लहरों की अन्तः-क्रीड़ा के कारण अकथनीय दुःख, क्षोभ, कष्ट और निराशा का सामना करना पड़ता है।
संवर्धन, परिवर्तन, जरा, मृत्यु आदि शरीर के सब विकारों के विविध अनुभव लेने के लिए जीव आबद्ध होता है। किसी भी अप्रिय वस्तु का सम्पर्क दुःख है। प्रिय वस्तु का अभाव दुःख है। अभीप्सित पदार्थ की अप्राप्ति दुःख है। अवांछित पदार्थ की प्राप्ति दुःख है। अन्ततोगत्वा, इन सबका वियोग दुःख का कारण है। महापुरुषों ने बन्धनों तथा अपूर्णताओं, व्याकुलता और अशान्ति तथा शक्ति, विषाद, क्लेशों से पूर्ण इस जीवन पर गहन चिन्तन किया। इस भौतिक जीवन के नाना प्रकार के क्लेशों पर निदिध्यासन करके उन्होंने कहा- "नहीं! इस भौतिक संसार में हमें जन्म-मृत्यु के पाश में पुनः पुनः नहीं फँसना चाहिए। अपनी लक्षित यात्रा को शीघ्र समाप्त करके पूर्णत्व एवं सर्वोच्च आनन्द की परम स्थिति को प्राप्त करने का साधन अवश्य खोजना चाहिए।
पूर्णत्व और समग्रता की अचिरेण प्राप्ति हेतु 'योग' साधना का विकास किया गया। यौगिक जीवन का अर्थ है-विकास की सघनता, क्योंकि योगी को मन्द गति, शिथिल क्रम अपेक्षित नहीं है। भारत में, अद्भुत परिपूर्ण चेतन तत्त्व से 'एकत्व' को योग की संज्ञा दी गयी है। अतः पुनः इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपका जीवन योगमय है, तो आप इस मनुष्य-जीवन-रूपी वरदान की अल्पावधि में ही वे कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं जो भविष्य के अनेक जन्मों में भी न कर सकते, जिनकी अवधि सहस्रों वर्ष भी हो सकती है। अतः योग का तात्पर्य यौगिक विकास द्वारा इसी जीवन में एक ही क्रम अथवा जीवन के कतिपय वर्षों में ही लक्ष्य प्राप्त करना है। यदि इस दृष्टिकोण से आप यौगिक जीवन पर दृष्टिपात करें, तो आप अनेक ऐसी बातें समझने लग जायेंगे जो आपके लिए सम्भ्रान्तक रही हों।
यदि कोई वनस्पति शास्त्रज्ञ अपनी कौसुमिक कार्यशाला (floral laboratory) में किसी ऐसे साधन का विकास करता जिसके द्वारा वह बीजारोपण के अनन्तर किसी भी फल के वृक्ष को तीन मास में वृक्ष-रूप दे कर छह मास में उससे फल प्राप्त कर लेता, तो एक चमत्कारपूर्ण और असामान्य कार्यपूर्ति हेतु वह निःसन्देह उस समय का महान् व्यक्ति कहलाता। सम्पूर्ण विश्व उसकी इस उपलब्धि से उत्सुक हो उठता। उसके अन्वेषण पर आधारित लेखों, उत्पादन के चित्रों का प्रकाशन होता, रोडियो और दूरदर्शन में उसके चमत्कार की कहानी के विवरण दिये जाते कि जिस कार्य की पूर्णता में पहले अधिक समय की आवश्यकता थी, वह अब विकास-क्रम में अपेक्षाकृत कम समय में सम्पन्न हो गया है।
पराकाष्ठा का नाम योग है
विकासशील व्यक्ति जो प्राप्ति दीर्घकालावधि में प्राप्त करता है, उन सब अनुभवों को अल्पावधि में समाहित करने के महान् प्रयत्न में अतीव असामान्य घटनाएँ तथा असामान्य दृश्य प्रकाश में आते हैं। तथाकथित व्यक्ति के चेतन में हो रही क्रिया से अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए यह बात असाधारण है; किन्तु ज्ञानी उनकी अभिव्यक्ति का कारण बन जाता है। सभी साधकों तथा योगाभ्यास करने वालों के जीवन में ऐसी घटनाएँ घटित नहीं होर्ती, प्रत्युत् केवल उन्हीं के साथ ऐसा होता है जो सर्वथा योग-पथ का अनुसरण करते हुए योग-जीवन में अपने प्रत्येक रोम-रोम, नाड़ी, हृदय से, मन से, बल से एवं आत्म-समर्पण भाव से प्रवृत्त हो जाते हैं।
योगी का पंचकोषों में परिवर्तन
विकास और उन्मीलन के इस क्रम में व्यक्ति के अपने अस्तित्त्व में पाँच विविध कोषों पर अनेक परिवर्तन आते हैं। अन्नमयकोष में विविध परिवर्तन और अनुभव दृष्टिगोचर होते हैं। मनोमयकोष (मन और प्राण) स्तर पर कुछ परिवर्तन आते हैं, स्वाभाविक क्रम में कुछ योग्यताएँ आती हैं और कुछ को विषयीपरक स्वगत के रूप में और शेष जनों को वास्तविक रूप में, कुछ दृश्य दिखायी देते हैं। तृतीयतः प्राणमयकोष में बौद्धिक स्तर पर कुछ घटनाएँ सूक्ष्म स्तर पर घटित होती हैं, जो मनोमय स्तर की अपेक्षा और भी सूक्ष्मतर हैं। चतुर्थ विज्ञानमयकोष आपका आध्यात्मिक स्तर है और आध्यात्मिक विश्लेषण द्वारा आपको अनेक आन्तरिक अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। यहाँ यह और अधिक विषयी परक है और घटित हो रही घटनाओं से जिज्ञासु ही अवगत होता है अन्य व्यक्ति नहीं, जो इसे जानने में असमर्थ है; क्योंकि यह और भी सूक्ष्म गहन स्थित है जो व्यक्ति की गहराई में है। पंचम आनन्दमयकोष परम चैतन्य का स्तर है। यह सार्वभौम चैतन्य, प्रभुचैतन्य है और इस स्तर पर जो दृश्य प्रत्यक्ष दृष्टिगत होते हैं, वे वास्तविक चमत्कार हैं जैसा कि सर्वविदित है। ईसामसीह इस स्तर पर पहुँचे और उनको जीवन में जो कुछ भी साक्षात् दृष्टिगत हुआ, वह इसी दिव्य तत्त्व के परम चैतन्य स्तर की शक्ति और महिमा थी। उन्होंने मनुष्य-रूप में नहीं, प्रत्युत् दिव्य शक्ति के रूप में चमत्कार दिखाये।
अतः योगी के अस्तित्व के पाँचों स्तरों पर चमत्कार साक्षात् रूप में दृष्टिगत होते हैं। लगन से योगाभ्यास आरम्भ करने, यौगिक मुद्रा और श्वासक्रियाएँ अथवा प्राणायाम में श्वास पर किंचिद् संयम आदि शारीरिक क्रियाओं पर ध्यान देने से आपको विविध रहस्यपूर्ण अनुभव प्राप्त होंगे।
सच्चे मन से, समुचित रूप से, योगासनों का अभ्यास करने का प्रयास करने तथा आसन-जय (आसनों पर विजय या सिद्धि) प्राप्त होने पर्यन्त अविरोध अभ्यास करते रहने से समय-समय पर असाधारण संवेदना की अनुभूति होती है। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि आपका भार एक टन है और आप घरती में धँसते जा रहे हैं और धरती स्वयं आपके भार से दबी जा रही है और आप इतने भारी हैं कि आपको उस स्थान से कोई हटा नहीं सकता। कभी-कभी इसके सर्वथा विपरीत अनुभव करते हुए पंख के समान हलका (बोझ रहित) अनुभव कर सकते हैं और तब आपको यह भी आभास नहीं होता कि आप बैठे हुए हैं। यह अनुभव आसन-जय उपलब्धि के उपरान्त साकार होते हैं; किन्तु यह अनुभव विषयीपरक हैं। अन्य अवसरों पर किसी ध्यानमुद्रा में बैठे हुए साधक को आकस्मिक कम्पन हो सकता है और पर्याप्त समय पर्यन्त बैठने पर साधक का स्वयं को प्रथम आसनस्थ स्थान से बहुत फुट दूर तक पाना कोई असाधारण बात नहीं है। यह वास्तविक लघुकरण नहीं है, साधक को कोई चोट नहीं पहुँचती और न ही साधक लघु चालन के प्रति सजग होता है। यह तो ऐसा अनुभव है जो दीर्घकाल पर्यन्त आसन करने वाला एक अथवा दो वर्ष में प्राप्त कर सकता है। इसी कारण से ही अनेक गुरुजन साधकों को उच्च स्थान, चट्टान आदि पर बैठने का आदेश नहीं देते; वरंच साधकों को फर्श पर कुछ बिछा कर बन्द कमरे में बैठने का आदेश होता है।
यह कैसे सम्भव होता है? हठयोग में शुद्धि पर अधिक बल दिया गया है। योग का अर्थ है-"शुद्धि के स्तर पर आरोहण ।" जब यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया कार्यान्वित होती है, शरीर के जीवाणुओं में और विविध आन्तरिक नाड़ियों के द्वारा मानसिक शक्ति में परिवर्तन आता है। ऐसा होने पर विविध आन्तरिक नाड़ियों के द्वारा मानसिक शक्ति में परिवर्तन आता है। शरीर में सत्त्व के प्रचुर मात्रा में प्रसार के कारण एक नवीन नाड़ी-प्रवाह गतिशील होता है जिससे शरीर में प्रतिक्रिया होती है और फलस्वरूप कभी-कभी शरीर में आकस्मिक कम्पन (झटकों) का अनुभव होता है।
कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ
सच्चे मन से अल्पमात्र की साधना करने वालों का प्रायः मनोमय स्तर पर ऐसा अनुभव रहा है (उन्होंने चाहे इसे योग के नाम से जाना है अथवा स्वेच्छा से विशेष आसनों के अभ्यास किये हों) उन्हें कुछ विशेष योग्यताएँ प्राप्त हुई हैं। इनमें से अत्यन्त प्रसिद्ध योग्यता अथवा चमत्कारिक अनुभव है— विचाराध्ययन! अर्थात् दूसरे के मन के विचार जान लेना। आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के बोलने से पूर्व ही आप उसके मन की बात जान लेते हैं। आप दूरभाष यन्त्र (टेलीफोन) उठा कर कुछ बात कहें और यह सर्वथा वही हो सकती है जो दूसरे व्यक्ति के मन में हो; बात करते समय आपको उस व्यक्ति के संवाद का पूर्व ज्ञान हो जाता है। अगले व्यक्ति के मन की बात आप पुनरुक्त करना प्रारम्भ कर देते हैं। इसे दूर-भाषण-विज्ञान (टेलीपैथी) कहते हैं। किन्तु यह विकसित दूर भाषण विज्ञान की अपेक्षा स्वतः प्रवर्तित (स्वेच्छामूलक) है। आचरण के समय आपको इसका ज्ञान भी नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं। यह स्वेच्छामूलक दूरभाषण प्रायः घटित होता है और चमत्कारिक क्रियाओं में यह सर्वप्रथम और कृतदृष्ट है। यह मनोमय स्तर पर आधारित है।
द्वितीय अनुभव है-दिव्य दृष्टि। यह भी सुविदित है। अनेक व्यक्ति दूरस्थित वस्तु को भी देख सकते हैं। तृतीय स्थान पर है- दिव्य श्रवण, जिसमें आप अकस्मात् ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं कि दो सौ मील दूर बोल रहे व्यक्ति को भी श्रवण कर सकते हैं।
दूरभाषण, दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रवण-तीनों चमत्कारिक प्रयोग निम्न स्तर पर हैं। प्राण के शुद्ध और मस्तिष्क के पवित्र हो जाने पर यह विषय स्वभावतः ही घटित होते हैं और प्रायः उनके प्रति व्यक्ति को स्वयं ज्ञान नहीं होता। कुछ व्यक्ति उनके प्रति सजग होते हुए भी यह नहीं जानते कि वे असामान्य शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों को वे अधिकार रूप में ले लेते हैं। जब कोई शक्ति शनैः शनैः किसी व्यक्ति में उत्तरोत्तर बढ़ती है, तो वह व्यक्ति इसके प्रति सचेत नहीं होता कि यह असामान्य है और इसे वह वरदान समझ बैठता है। योग में ये तीन शक्तियाँ मौलिक हैं-योग-पथ में प्रारम्भिक चमत्कार-अन्य विधियों की अपेक्षा योग में यह अधिक तीव्रता से विकसित होते हैं।
किंचिदधिक उन्नति करने पर प्राणी की विद्युत्-शक्ति जागृत होती है, जब कि मनोमय स्तर से आगे सूक्ष्म स्तर का उन्मीलन भी प्रारम्भ हो जाता है और अन्य शक्तियों का विकास होने लगता है। आपके हस्त-मार्जन द्वारा कोई व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। आप ऐसे कक्ष में प्रवेश करें जहाँ कोई व्यक्ति व्याकुल मनःस्थिति में बैठा हो और उसकी व्याकुलता लुप्त हो जाये, साधक के समीप कोई अत्यन्त क्रुद्ध व्यक्ति आ जाये जो अपशब्द कहने को उद्यत हो, किन्तु साधक को देख कर वह मूक हो कर लौट जाये-ऐसा सम्भव हो सकता है। इन गुणों का विकास होने पर रोगहरण तथा तत्काल किसी व्यक्ति को वशीभूत करने की शक्तियाँ मनुष्य में आ जाती हैं—यह सूक्ष्म स्तर पर हैं। यह शक्तियाँ यथार्थतः आध्यात्मिक स्तर पर नहीं हैं; किन्तु अभ्यास में अल्पमात्र भी उन्नति करने पर इनका उद्विकास प्रारम्भ हो जाता है।
शुद्ध चमत्कार की क्रिया योग नहीं
यहाँ एक सत्य की पुष्टि करना आवश्यक है जिसके प्रति आपको सजग रहना है। मनोमय स्तर, प्राणमय स्तर, मन और प्राण एवं सूक्ष्म स्तर (बुद्धि) से प्राप्त होने वाली शक्तियाँ आप थोड़े प्रयास से ही उपलब्ध कर सकते हैं। यदि धारणा की जाये, तो आवश्यक प्रयास का विकास किया जा सकता है। योग में वे शोधन द्वारा उपलब्ध होते हैं और द्वितीयतः वे संकल्प-शक्ति, अभ्यास और अनवरत यत्न द्वारा प्राप्त होते हैं जैसा कि अभी इसका वर्णन आया है। दूरदर्शन, दिव्य भाषण, दिव्य श्रवण आदि शक्तियाँ, सम्मोहन शक्ति एवं कृत्रिम निद्रा के प्रयोगकर्ताओं में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती हैं और अन्य जनों में, जिनके जीवन शास्त्रनीति से सर्वथा विपरीत हैं, जो जिज्ञासु नहीं हैं और जो योग के नियमों, शुद्धता, आत्म-संयम, प्रभु-भक्ति, विश्वास आदि के प्रतिपालक नहीं हैं, यह शक्तियाँ देखी जाती हैं। सुषुप्तिजनक और सम्मोहन शक्तियों से युक्त कतिपय सामान्य एवं मात्र चमत्कारी व्यक्ति विशेष ऐसे भी हैं जिन्होंने चमत्कार को ही अपना प्रमुख व्यवसाय बना लिया है। इस प्रकार से उपलब्ध शक्तियाँ उनकी प्रकृति के विकास अथवा आध्यात्मिक स्तरीय उन्नति को लक्षित नहीं करर्ती; क्योंकि यदि ये शक्तियाँ, अद्वितीय सत्य वास्तविक जीवन का ध्येय एवं परम लक्ष्य परमात्मा में गहन तथा स्थायी विश्वास पर आधारित सत्य को साक्षात्कार करने के अभिप्राय से उपलब्ध नहीं की गयीं, तो यह योग नहीं हैं।
हममें से प्रत्येक का ब्रह्म मनस् से सम्बन्ध है; क्योंकि हम सबका स्रोत वही है, हमारा चैतन्य 'ब्रह्म चैतन्य' का अंश है और हमारा मन 'ब्रह्म मनस्' का अंश है, किन्तु दोनों का सम्पर्क नहीं है। उसका विच्छेद हो गया है। क्यों? क्योंकि हम अपने ही अहं के पाश से बंधे हुए हैं। किन्त जब हम इससे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, तो हमारी चेतना को ब्रह्म चैतन्य से और हमें ब्रह्म मनस् से मिलाने वाला संकीर्ण पथ और भी निर्मल होने लगता है और हम अपने अस्तित्व की एकता को अनुभव करने लगते हैं। ऐसा होने पर सामान्य मन से छिपा ज्ञान हमारे अधिकार में आ जाता है, दूरस्थ घटनाओं एवं वस्तुओं का ज्ञान और कभी-कभी तो भविष्य का ज्ञान भी होने लगता है। इसका कारण चैतन्य का विस्तार है, जब एक विकास के विशेष स्तर तक पहुँचने पर आभ्यन्तर आध्यात्मिक तत्त्व गतिशील हो जाता है और आत्मिक प्रकृति जागृत हो जाती है।
परमात्मा की प्रथम सृष्टि सूक्ष्म तत्त्वों से सम्पूर्ण निरूपित विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है। सूक्ष्म तत्त्व हैं- अन्तरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनमें आकाश सूक्ष्मतम है। इन सूक्ष्म तत्त्वों में स्थूल तत्त्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए; क्योंकि वे अत्यन्त सूक्ष्म नियम अथवा आधारभूत पराभौतिक आदि तत्त्व हैं जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मैं इहलौकिक अग्नि, वायु, जल और आकाश का वर्णन नहीं कर रहा, प्रत्युत् सूक्ष्मतम सारतत्त्व की विवेचना कर रहा हूँ जिनसे दृष्टिगोचर (प्रत्यक्ष) ब्रह्माण्ड की रचना हेतु स्थूलतर अभिव्यक्तियाँ परिस्फुटित हुई हैं। इन स्थूल एवं भौतिक तत्त्वों का स्रोत अदृश्य, सूक्ष्म तथा जगत् सम्बन्धी है। राजयोग के अभ्यास-क्रम में योगी जब इन सूक्ष्म तत्त्वों में से एक या अधिक पर एक-साथ एकाग्र, ध्यानस्थ एवं समाधिस्थ होने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तब वह इन पंच महाभूतों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। वह विद्युत्-वेग से अन्तरिक्ष में भ्रमण कर सकता है, अग्नि अथवा जल के ऊपर खड़ा हो सकता है; क्योंकि इन महाभूतों के मूलरूप पर उसे सम्पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त है।
विशेष योगियों की इनमें क्षमता असामान्य घटना है। अग्नि और जल से हो कर आते हुए भी वे अप्रभावित प्रतीत होते हैं। पंच महाभूतों पर संयम ही इसका कारण है।
कुण्डलिनी से खेलना अग्नि से खेलना है
जब आपका आध्यात्मिक अभ्यास कुण्डलिनीयोग का रूप धारण करता है और आप आभ्यन्तर अलौकिक क्रम हठयोग प्रारम्भ करते हैं; तब प्रत्येक प्राणी के अद्भुत देह में स्थित निम्न रहस्यपूर्ण चक्रों से कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने के साथ ही विविध असामान्य शक्तियाँ और अनुभव जागृत होते हैं; क्योंकि ब्रह्माण्ड के अन्तर प्रदेश में रहस्यपूर्ण मण्डल हैं और प्रत्येक चक्र कुछ रहस्यपूर्ण मण्डलों पर अनुशासन करता है और उन मण्डलों का दृग्विषय साधक का अनुभव बन जाता है, जब वह इस कुण्डलिनी-योग के पथ पर आरूढ़ हो कर उस चक्र-विशेष पर प्रयोग करने की चेष्टा करता है। मैं कुण्डलिन-योग का सदा अपवादक रहा हूँ। इस बीसवीं शताब्दी में आधुनिक पुरुषों में से अधिकांश के लिए तो कुण्डलिनी योग उचित ही नहीं। मैं तब तक आपको इस विज्ञान के समीप जाने का आदेश नहीं देता, जब तक आपको किसी ऐसे सिद्ध गुरु के सान्निध्य का विलक्षण सौभाग्य प्राप्त न हो, जिसने कुण्डलिनी योग से आत्म-प्रकाश प्राप्त किया हो। जब लोग इन आन्तरिक चक्रों के बारे में मुझसे प्रश्न करते हैं, तो मैं सदा यही कहा करता हूँ- "इसे न जानने में आपको कोई हानि नहीं।" कुछ ज्ञान उसे अपने लिए ही छोड़ देना हितकर है, उसे न जानना अधिक हितकर है। कुण्डलिनी-योग प्रचण्ड विधि है, हठयोग की विधि है जिसमें विशेष गुप्त शक्तियों को बलात् जागृत करने का प्रयास किया जाता है। योग प्रबल उद्भेग (परिणाम) की विधि है। कुण्डलिनी योग इस विधि में और अधिक प्रबल है, अतएव यह भयप्रद है। अग्नि से खेल है।
योग के सभी मार्गों में- चाहे वह परमात्मा के लिए पवित्र भक्तियोग हो (प्रार्थना द्वारा), विश्वास (निष्ठा), पूजा, नाम, जप, भक्ति अथवा समर्पण द्वारा अथवा ज्ञानयोग (विवेक, श्रवण, गुरु के वचनों पर मनन और परम सत्य पर गहन ध्यान का दार्शनिक योग) अथवा राजयोग में (धार्मिक जीवन के अष्ट-गुण-उत्थान, दैनिक धार्मिक अनुष्ठान-व्रत, आसन की स्थिरता, श्वास पर संयम, मन का संहरण, एकाग्रता, ध्यान एवं परम चैतन्य) अथवा कर्मयोग में (हार्दिक्क नम्रता से सबकी सेवा, अहंकारशून्यता और स्वयं को भगवान् का निमित्त मानते हुए दिव्य शक्ति को सम्पूर्ण आत्म-समर्पण, विश्व में, मनुष्य में और मनुष्य के द्वारा भगवान् की निःस्वार्थ सेवा और उपासना के द्वारा प्रभु-चरणों में अपनी समस्त सेवा अर्पित करना) - कुण्डलिनी का जागृत होना और इसका एक चक्र से दूसरे चक्र में आरोहण तात्कालिक क्रिया है, जब तक कि कुण्डलिनी अपने सर्वोच्च चमत्कारिक केन्द्र तक नहीं पहुँच जाती। ज्ञानी में, राजयोगी में, भक्त में और कर्मयोगी में तथा अन्य सब (योगियों) में यह क्रिया और कुण्डलिनी शक्ति की जागृति तथा निम्नतम केन्द्र से उच्चतम केन्द्र तक इसका शनैः शनैः आरोहण साधक के गुप्त अलौकिक व्यक्तित्व में क्रियान्वित होता है; अतः यह ऐसी क्रिया है जो स्वतः ही क्रियान्वित होती है। किन्तु आप यदि जानते हुए भी किसी विशेष बलवत् विधियों से उसे जागृत करने का यत्न करेंगे, तो मैं कहता हूँ-सदा ही ऐसी शक्तियों के उठने का भय है जिनका आप सामना नहीं कर सकते; क्योंकि आपका व्यक्तित्व उनके साथ एक होने अथवा उनमें लीन होने के लिए इतना पवित्र नहीं है। अन्य योग-मार्गों में, उन्नति के साथ आपके व्यक्तित्व में पूर्ण परिवर्तन और सम्पूर्णता का आभास होता है। हठपूर्वक कुण्डलिनीयोग में प्रायः ऐसा होता है कि व्यक्ति उस विधि में सम्पूर्ण शक्ति लगा देता है और आधारभूत मौलिक नियमों की उपेक्षा करने लगता है, अनिवार्य तैयारियों की उपेक्षा करता है। एवंविध साधक के तैयार होने से पूर्व ही इन शक्तियों का उन्मीलन हो जाता है। कुण्डलिनीयोग एक यथार्थ विद्या है और इसकी युक्तियाँ अचूक हैं; किन्तु उनका विधिवत् पालन अनिवार्य है। इस प्रकार अत्यधिक शक्ति प्राप्त होने पर साधक उसका प्रयोग करने में असमर्थ हो जाता है। वह उसे सहन भी नहीं कर सकता। अन्ततोगत्वा, उसके लिए पूर्ण यौगिक जीवन समाप्त हो जाता है।
कुण्डलिनीयोग में ही असाधारण सिद्धियाँ अलौकिक तत्त्व और यह सब अलौकिक अनुभव उग्ररूपेण अनावृत होते हैं; क्योंकि यह आपमें विद्यमान सर्वोच्च शक्ति को जागृत करने की वैज्ञानिक कला है। योग के अन्य मार्गों में शुद्धि के द्वारा आपके व्यक्तित्व के विभिन्न आध्यात्मिक केन्द्रों में सुप्त शक्तियाँ अन्तिम चरण तक प्रकट होती हैं और तब ब्रह्म-चैतन्य द्वारा आप सब दिव्य शक्तियों से सम्पन्न हो जाते हैं, इसके उपरान्त आप सर्व-समर्थ हो जाते हैं। सिद्धि द्वारा जब आप योग के अन्तिम चरण में पहुँचते हैं, तो आपको महान् सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जैसे 'अणिमा' (अति सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता), 'महिमा' (विशाल रूप धारण करने की क्षमता), 'लघिमा' (लघुत्व), गरिमा (भार में असाधारण गुरुत्व) आदि। उदाहरणतया लघिमा को ही लीजिए। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यदि एफिल टावर अथवा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से गिराया जाये, तो वह गिरने की अपेक्षा धरती की ओर पंख के एक टुकड़े की भाँति तैरने सा लगेगा। योगियों द्वारा इन शक्तियों का आवेक्षण-आधीन प्रदर्शन हुआ है। ऐसा सुना गया है कि एक योगाचार्य ने अमेरिका-वास के अपने प्रारम्भिक दिनों में गरिमा का प्रदर्शन किया। वह यह दिखाना चाहता था कि उसके पास केवल अर्जित ज्ञान ही नहीं था। उसके प्रवचन का विषय अनुभव एवं सत्य पर आधारित था। कभी-कभी जन-भावना (जनगण में भाषण करते समय) में वह यौगिक शक्ति को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रदर्शन किया करता था। दृष्टान्तरूपेण, वह बैठ जाता और श्रोतागणों में से किसी का आह्वान करता जो उसे उठाने का यत्न करता और ऐसे अवसर आये जब कि एक नहीं प्रत्युत् अनेक व्यक्तियों ने सम्मिलित रूप से उसे उठाने का प्रयास किया; किन्तु असफल रहे। एक बार एक अत्यन्त भारी शक्तिशाली पुलिस कान्सटेबल ने उस योगी युवक को हिलाने का प्रयत्न किया जो उस समय इतना भारी नहीं था; परन्तु कान्सटेबल उसे एक बाल की चौड़ाई तक भी नहीं हिला सका। यह प्रदर्शन न्यूयार्क (अमेरिका) शहर में पाँच-छह सौ लोगों के समक्ष किया गया। यह सब घटनाएँ यौगिक उन्नति के अन्तर्गत आती हैं।
गुप्त शक्तियों से सम्पन्न व्यक्ति
प्रभु की अपार कृपा से कुछ अलग प्रकार की रहस्यमयी शक्तियाँ कभी-कभी ऐसे पुरुष को भी प्राप्त हो जाती हैं, जिसने कभी यौगिक अनुष्ठान किया ही न हो। ऐसा तभी होता है, जब ईश्वर किसी पुरुष को किसी भी दिव्य प्रयोजन से निमित्त बनाना चाहता है, और वह ऐसा दृष्टिगत होता है जो आजीवन सच्चारित्र्य की पराकाष्ठा द्वारा योग्य एवं उचित साधन सिद्ध हुआ हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सदा एक असाधारण नम्रता और अहं-लोप से संलक्षित होता है और वह इन शक्तियों का स्वेच्छा से प्रयोग नहीं करता। 'मैं' (अभिमान) सर्वदा एक ओर रहता है और ऐसा व्यक्ति सदा इच्छित एवं अहं-भाव रहित साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा व्यक्ति सदा पूर्णरूपेण अनासक्त होता है और इस संसार की किसी देन के पीछे नहीं भागता । वह अत्यन्त सादगी का, प्रायः निर्धनता का जीवन व्यतीत करता है। अत्यधिक नम्रता और अनासक्ति ऐसे व्यक्ति के चरित्र की मुख्य विशेषताएँ बन जाती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम हैं; परन्तु ऐसी स्थिति असम्भव नहीं है। इस तथ्य का आपको ज्ञान कराने के। लिए मैंने यह विवरण दिया। भारत तथा अन्य देशों में भी ऐसे दृष्टान्त हुए हैं, जब प्रभु-कृपा से योग्य पुरुष में सहसा ही शक्तियों का आविर्भाव हुआ।
चमत्कारिक शक्तियाँ और जिज्ञासु
ऐसी विभिन्न शक्तियों का योग में क्या स्थान है? उनके लाभ-अलाभ क्या हैं? इन शक्तियों के प्रति सच्चे साधक का दृष्टिकोण कैसा है? इन शक्तियों के प्रति गुरुजनों का क्या दृष्टिकोण है? योगी के जीवन में इन शक्तियों तथा विभिन्न अनुभवों का क्या स्थान है?
प्रथम स्थान में इनके प्रति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञातव्य तथ्य यह है कि वे शक्तियाँ जन्म से ही साथ आती हैं। वे योगी की इच्छा नहीं होतीं। वे ऐसी वस्तु नहीं हैं जिसके लिए साधक ने खोज प्रारम्भ की हो। उसके लिए वे राह में अतिक्रमणीय पदार्थ हैं। जिस प्रकार आप नगर की ओर यात्रा पर चलते हैं और एल्डोरेडो, मॉटल, सिम्पसर्स सियर्स और फिर एक पुल पार करते हैं, सबका उल्लंघन करना है; क्योंकि उनमें से कोई भी आपका गन्तव्य नहीं जिसके लिए आप चले थे। आप पूछ सकते हैं- "यह सब चीजें (राह में) क्यों आती हैं?" अस्तु! आप आगे बढ़ रहे हैं, आप स्थानान्तर गमन कर रहे हैं, आपको पथ में अथवा महापथ के मध्य आने वाली सब वस्तुओं का उल्लंघन करना है, आप उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का यह विश्वस्त लक्षण है।
द्वितीयतः वे प्रोत्साहन का कार्य करती हैं। अन्ततः एक मानव की यह जिज्ञासा होती है कि वह कुछ कार्य सम्पन्न कर रहा है अथवा उसके प्रयास निष्फल ही जा रहे हैं। वे उचित एवं यथार्थ हैं अथवा उसके प्रयास निष्फल ही जा रहे हैं। वे उचित एवं यथार्थ हैं अथवा विमार्गदृष्ट एवं निरर्थक हैं-इति!
ये शक्तियाँ आपके आदर्श चरित्र की परीक्षा लेने के लिए प्रलोभन के रूप में सामने आती हैं और आत्म-ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। ये शक्तियाँ इतने सूक्ष्म रूप से छल से आपमें प्रविष्ट होती हैं कि जब आप असाधारण रूप से अन्तर्दर्शी, असामान्य रूप से सजग और अतीव सावधान न रहें, आप उनके वशीभूत हो कर विफल हो सकते हैं और आपको इस बात का ज्ञान भी न होगा। इसके पश्चात् मनुष्य में एक अन्य प्रकार का अहं-भाव जागृत होता है जो किसी भी स्थूल अहंकार से निकृष्टतर होता है जैसे-पद का, धन का, यौवन अथवा यश एवं शक्ति का अभिमान। यह अभिमान उच्च होने तथा अन्य मानव जाति से ऊपर रहने का है।
"अन्य जनों के पास वह वस्तु नहीं है जो मेरे पास है" इस प्रकार का तुच्छ खोखलापन और अहंकार सर्वोच्च बाधा है। यह साधक के लिए सबसे बड़ा खतरा है; क्योंकि यह अभिमान को पुष्ट करता है जो उसका घोर शत्रु है। भगवद्-प्राप्ति हेतु इस 'अहं' का विनाश करना होगा। 'अहं' को प्रोत्साहित करने वाली प्रत्येक वस्तु परमात्मा की विरोधी है। आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शैतान आपके भीतर प्रवेश करके आपको ये शक्तियाँ प्रदान करता है। शैतान जब आपको वशीभूत कर लेता है, तब ये शक्तियाँ आपमें आ जाती हैं। आध्यात्मिक रूपक के शब्दों में-आपने जो सिंहासन परमात्मा के लिए बनाया उस पर अब शैतान ने अधिकार कर लिया है। अतः ये शक्तियाँ आपको सुपथ से दूर ले जाती हैं और आपके मिथ्या अहं को उन्मत्त करती हुई आपको परमात्मा से विमुख करती हैं।
जिज्ञासु को अत्यन्त सजग रहना चाहिए ताकि वह इन शक्तियों को कदाचित् प्रोत्साहित न करे, इनके विचार मन में न लाये और इनका सर्वथा त्याग करे।
इन शक्तियों के प्रति आचार्यों का क्या मत है? सभी योगाचार्य-सबसे बड़े आचार्य, मेरे गुरु श्री स्वामी शिवानन्द, आज के युग के महान् सन्त स्वामी रामकृष्ण-स्वामी विवेकानन्द के गुरु जो १८९३ में अवतरित हुए और संसार को योग और वेदान्त का ज्ञान दिया तथा अन्य सन्तगणों का भी इस विषय के प्रति सर्वथा एकमत है। वे कहते हैं: "आध्यात्मिक पथ के अनुसरण में प्रारम्भ से ही मनोमय (आध्यात्मिक) शक्तियों से सावधान रहो, चमत्कारिक शक्तियों से सावधान रहो!" उनके इन्द्र जाल में फँस कर आप स्वयं को खो देंगे। आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जायेगा और आपका सब योग सरलता से समाप्त हो जायेगा। और एक बार योग के खो देने पर इसे पुनः प्राप्त करना अत्यन्त ही कठिन है। प्रायः इसकी पुनर्प्राप्ति असम्भव ही होती है। एक बार योग से पतित होने पर खोयी हुई स्थिति प्राप्त करने में निश्चयेन बहुत समय लगता है। उपेक्षावृत्ति में आचार्य अत्यन्त दृढ़गत हैं। वे कहते हैं- “विष के त्याग की भाँति चमत्कारिक शक्तियों का परित्याग करो।" आत्म-जागृति में वे विष के समान ही हैं। उनको एक ओर कर दो।
श्री रामकृष्ण को इसका वास्तविक अनुभव था। उन्होंने कहा- "एक बार ये शक्तियाँ उनके पास एक टोकरी में लायी गयीं। यह आन्तरिक चमत्कारिक अनुभव था जिसमें उन्हें यह भेंट प्रदान की गयी और स्वीकार करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। प्रथम दृष्टि में वे सत्य प्रतीत हुईं और वे उन पर दृष्टिपात करने वाले ही थे, जब अनायास ही सम्पूर्ण वास्तविकता का उन्हें ज्ञान हो गया कि वे चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, मायावी शक्तियाँ हैं, समस्त पृथ्वी का राज्य, उन्होंने तत्काल ही उन पर थूक दिया। भारत में थूकना निकृष्टरूप तिरस्कार माना जाता है और उन्होंने थूक कर चिल्लाना प्रारम्भ कर दिया-“इन्हें दूर ले जाओ, उन्हें इसी क्षण दूर करो।" समीपस्थ जनगण भागे आये और पूछने लगे-"क्या बात है? क्या हो गया है?" वे शान्त हो गये। स्वयं को संयमित किया। पश्चात् काल में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की शक्ति उनको अर्पण की गयी और क्षण-भर के लिए प्रायः मन ने उन पर दृष्टिपात किया -"परन्तु मेरी 'माँ' मेरी रक्षा करने के लिए आयी और मैं उनको एक ओर हटाने में पूर्णतया समर्थ हो गया।" अतएव आरम्भ काल से ही आचार्यों का आदेश यही रहा है कि यदि आप परब्रह्म परमात्मा को चाहते हैं, तो सभी शक्तियों का उसी प्रकार त्याग करो जिस प्रकार आप विष का परित्याग करते हैं। चमत्कारों के जाल में मत फँसो और इनसे विचलित भी न होओ, अन्यथा इनके ज्ञान से पूर्व ही आप इनके वशीभूत हो जायेंगे। यदि आप ईश्वर-प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं, तो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ की आकांक्षा न करो; क्योंकि ईश्वर-प्राप्ति पर सर्वस्व-प्राप्ति हो जाती है। मुझसे सीख लो। आपके पास परब्रह्म है, तो सर्वस्व है। विश्व में आपको किसी प्रकार के अभाव की प्रतीति न होगी। ब्रह्म के अतिरिक्त प्रत्येक पदार्थ भस्म-रूप दृष्टिगोचर होगा; क्योंकि मूलतः वे किंचिद् मात्र भी नहीं। ईश्वर चाहिए तो महत्तम, उच्चतम, मधुरतम, अनन्त की ओर बढ़ो। अन्य किसी पदार्थ की अल्पमात्र भी कामना न करो और ये चमत्कारी शक्तियाँ यदि मार्ग में आयें, तो इनकी उपेक्षा करो। विचलित नहीं होना चाहिए; क्योंकि यौगिक पथ पर उन्नति तभी प्राप्त होती है, जब आप पूर्ण मन से सम्पूर्ण व्यक्तित्व लगा कर इसे करते हैं। हृदय, मन और व्यक्तित्व की पूर्णरूपेण शत-प्रति-शत संलग्नता अनिवार्य है। कोई भी विक्षेप, जिसमें आप खो जाते हैं, आपकी उन्नति में विलम्ब का कारण बन जाता है।
अन्ततः, चमत्कारिक शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग क्या हैं? इसके दोषों का वर्णन तो स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। उनका प्रयोग करना, उनके वशीभूत हो जाना-स्वयं में यह बहुत बड़ा दोष है; क्योंकि उनका प्रयोग वर्जित है। इस बात का भी भय रहता है कि आप नम्रता, अच्छाई, सत्य, दया, प्रेम, कृपा आदि का जो सच्चरित्र स्थापित करते हैं, वह आधार रूप में सदाचार के अभाव में ईश्वर को पूर्ण आत्म-समर्पण न करने, पग-पग पर उसके पथ-प्रदर्शन की अभिलाषा रखने और निरन्तर प्रार्थना द्वारा सात्त्विक जीवन को पुष्ट न करने का और उस परमात्मा को हृदयोन्मुख न करने से, इन शक्तियों द्वारा सहज रूप से प्रभावित हो सकता है। पुनश्च, मनुष्य यदि सबल नहीं है और एकत्रीकरण में ही रत है, तो ये शक्तियाँ आ कर मन को • कलुषित करती हैं और मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के प्रारम्भ में व्यक्त पदार्थों की पुनर्प्राप्ति हेतु उन शक्तियों का प्रयोग करने लगता है। यदि शक्तियाँ प्रयोग की जायें, तो मनुष्य सम्पत्ति का, भोग-विलास का, आसक्ति का, अधम एवं पाशविक वृत्तियों का दास बन जाता है। ऐसा कथित है कि प्रलोभनों के अभाव में मनुष्य सदाचारी रह सकता है; किन्तु प्रलोभन आने पर सात्त्विकता अन्तर्धान हो जाती है।
अतएव, प्रारम्भ में अतीव सजग रहने की आवश्यकता है; क्योंकि इन चमत्कारों में वशीकरण की शक्ति होती है।
चमत्कारों के प्रयोग
साधक, जिज्ञासु एवं ब्रह्म के इच्छुक, आत्म-साक्षात्कार हेतु ही जीवन को प्रयोग में लाने का प्रयास करने वाले मनुष्य इन शक्तियों का सर्वथा उपयोग नहीं करते। सच्चा साधक उनकी उपेक्षा करता है; क्योंकि उसके लिए वे सन्तोषप्रद और अमोघ नहीं हैं, प्रत्युत् मध्य राह में ही दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थ हैं।
पुनरपि, साधक की इन शक्तियों का यदि मैं स्वेच्छा से वर्णन करूँ, तो इन शक्तियों के कतिपय सीमित प्रयोग भी हैं। किसी ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना कीजिए जिसे ब्रह्म-जिज्ञासा सर्वथा नहीं है; किन्तु वह उपशमन (रोगहर) सम्मोहन-शक्ति से युक्त है और सिद्ध पुरुष है। दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रवण द्वारा वह भविष्य की बातों को बता सकता है-ऐसे अवसर पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है; किन्तु यह देखा गया है कि ऐसी स्थिति में शक्तियों का प्रयोग किये जाने पर कुछ कालोपरान्त वे लुप्त हो जाती हैं।
सम्मोहन शक्ति वह है जिसके द्वारा सिद्ध पुरुष किसी की चिकित्सा करके रोगहरण करता है। ज्योतिष ज्ञान द्वारा लोगों को सहायता प्राप्त हो सकती है। भविष्य में घटित होने वाली विपत्ति के पूर्व-ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति को उसकी विपत्ति के प्रति सावधान करके उसकी सहायता की जा सकती है। इन सीमित उपयोगों में व्यक्ति जो सच्चा साधक कदापि नहीं है, इन शक्तियों का दया, प्रेम अथवा स्वेच्छावश निःस्वार्थ-भाव से परोपकार हेतु उपयोग कर सकता है, कुछ व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करके आते हैं जैसे "मैं यहाँ आया हूँ। ईश्वर की इच्छा है कि मैं यह कार्य करूँ। मुझे ऐसा करना ही है।" और यदि कोई व्यक्ति इस धर्मार्थ प्रेरणा के साथ ही उपयोगी चमत्कारिक शक्तियों से भी युक्त हो, तो इसका अभिप्राय है कि किसी निमित्त हेतु उसे ये शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं और उसी निमित्त हेतु उनका प्रयोग होना चाहिए। किन्तु ऐसा व्यक्ति भगवद्-प्राप्ति नहीं कर सकेगा। उसके लिए उसे पुरुषार्थ करना होगा। एक अत्यन्त उत्कृष्ट स्तर पर इन चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। ये शक्तियाँ आचार्यों के पास रहती हैं जो विशेषतया आध्यात्मिक साधकों का पथ-प्रदर्शन करके उन्हें ईश्वर की ओर आसक्त करते हैं और इस प्रकार लोगों को सुमार्ग-दर्शन कराते हैं। कभी-कभी आचार्य गण ऐसे साधक में विश्वास की जागृति हेतु इन शक्तियों का उपयोग करते हैं जो प्रत्युत्पन्नमति है; किन्तु अविश्वास उसे पथ से विचलित कर रहा है। कदाचित् आचार्य सामान्य जनों की भी सहायता करते हैं। वे उन्हें कर्मानुभूतियों के अतिक्रमण का साधन बनाते हैं। वे उनके संचित कर्मों से तो उन्हें मुक्त नहीं कर सकते; परन्तु इन शक्तियों द्वारा कर्मों के दुःखों को अतिक्रमण करने में अवश्य सहायी होते हैं। एक अत्यन्त उच्च स्तर पर, कदाचित् इन शक्तियों का प्रयोग स्थूल परिमाण में, एक नहीं अनेक व्यक्तियों से युक्त क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए किया जाता है। ऐसी घटनाएँ हैं, जब आचार्यों ने बाढ़ पीड़ित अथवा अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशमनार्थ इन शक्तियों का उपयोग किया है; किन्तु हम इनसे प्रत्यक्षरूपेण सम्बद्ध नहीं हैं, क्योंकि ऐसे आचार्य स्वयं ही एक स्तर के ज्ञाता हैं और 'ईश्वरेच्छा' की पूर्ति हेतु वे शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
चमत्कारिक शक्तियों का परित्याग करो
निम्न स्तर पर ये शक्तियाँ सच्चे साधकों के लिए सबसे बड़ी विघ्न-रूप और पतन का कारण सिद्ध हो सकती हैं। अन्ततोगत्वा साधक को आत्म-साक्षात्कार करना ही है और एक बार अपने ही विवेक द्वारा जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर के अतिरिक्त सर्वस्व नश्वर है, क्षणिक है, आभास मात्र है, एक क्षणिक वस्तु है जिसके साथ किसी का शाश्वत सम्बन्ध नहीं है, तब उस परम शक्ति के अतिरिक्त धूल के अल्प कण से ले कर सर्वोच्च शक्तियाँ, सब चमत्कारी क्रियाएँ, गुप्त अनुभव निःसार हो जाते हैं। वे सभी गमनशील, नाशवान्, क्षणिक संसार के अंशभागी हैं। वे यथार्थ नहीं हैं। वे सत्य नहीं हैं और उनका आत्यन्तिक मूल्य नहीं है। वे अल्प मूल्य (असार) हैं।
अतएव प्रतिबिम्ब का अनुगमन मत करो। सार-तत्त्व का अवलम्बन लो। भूसे की इच्छा मत करो। पुष्टिप्रद, जीवनप्रद धान की इच्छा करो। असत्य ब्रह्माण्ड के पदार्थों के लिए सत्य-पथ से विमुख न होओ। सत्य को ही देखो, असत्य के मोह-जाल में मत फँसो। आपके अस्तित्व के उच्चतम, महत्तम, अन्तस्तम केन्द्र ईश्वर के अतिरिक्त सर्वस्व असत्य लोक से सम्बद्ध है। इन सब पदार्थों के प्रति सर्वथा विमुख हो कर अनन्य साधक को केवल ईश्वर का चिन्तन करना चाहिए। केवल ईश्वर के लिए जिओ। ईश्वर से ही प्रेम करो। महान् सत्य ईश्वर-केवल ईश्वर की ही एकाग्रचित्त हो कर आकांक्षा एवं अनुसन्धान करो। सभी शक्तियों के परिहार के लिए आचार्यों का यही सन्देश है।
केवल ईश्वर की ही आकांक्षा करो, ईश्वर से अन्यतर लेशमात्र भी कहीं विभ्रमित नहीं होना।
प्रभु की अनुकम्पा आपकी बुद्धि को प्रकाशित करे। आपके हृदय में परमात्मा का प्रेम भर जाये। महान् आचार्यों के आशीर्वाद आपकी अन्तरात्मा को सत्य, जागरूकता एवं विवेक की ज्योति से विभासित करें। आचार्य गण आपका पथ-प्रदर्शन करें। वे आपको सच्चे विवेक से युक्त करें! वे आपको आभ्यन्तर आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें जिससे आप सुपथ से विमुख कराने वाली तुच्छ चमत्कारिक शक्तियों के मोह और प्रलोभनों का अतिक्रमण कर सकें। वे आपको प्रेरणा दें, बल दें, परम आनन्द के लक्ष्य की ओर अग्रसर करें और दिव्य साक्षात्कार, अनन्त आनन्द, शाश्वत चैतन्य और ज्योति तथा अप्रमेय दिव्य शाश्वत और अबोधगम्य शान्ति की सर्वोच्च उपलब्धि से आपके जीवन का अभिषेक करें। भगवान् आपको आशीर्वाद दें और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे।
३. ध्यान
ज्योतिर्मय अमर आत्मन् ! प्रकाश एवं अमरत्व की धन्य सन्तति! दिव्य पथ के प्रिय साधको! हम अत्यन्त भाग्यशाली हैं जो प्रातः की इस वेला में दिव्य नाम और ध्यान की कीर्तिमयी धारा में स्नानार्थ एकत्र हो सके हैं। यह वेला प्रभु-प्रदत्त उपहार है। शाश्वत काल से हमारे स्रोत उस प्रभु की ओर से प्रेम की वृष्टि है जो हमारा परम धाम है और जिसमें हम सब एक हैं। ऐसा उपहार हमें प्रेम से अंगीकार करना चाहिए। प्रणिपातेन इसे स्वीकार करके भक्ति-भाव से इसका सदुपयोग करना चाहिए। वस्तुतः हम पर प्रभु की अनवरत दया एवं सच्ची कृपा के अभिज्ञान का लक्षण यही होगा कि हम स्वयं को उनकी कृपा के इन भावों को योग्य बनाने का सतत प्रयास करते रहें। इस प्रकार हम उसी मात्रा में परमात्मा के समीपस्थ होते जायेंगे। हमें स्वयं भी इस भाँति जीवन यापन करना चाहिए कि वह अन्तर्वासी परमात्मा (जो हमारी सच्ची आकांक्षाओं और हमारी अन्तस्थ इच्छाओं का ज्ञाता है) अपने मन में सोचे- 'मेरा यह वत्स इस मर्त्य भूतल के खिलौनों से विरक्त हो गया है। अधम, गमनशील एवं नश्वर पदार्थों से इसे अरुचि हो गयी है, मेरी इस महान् लीला के दृश्य, नाम और रूपों से तथा जीवन के नाटक से परिश्रान्त हो गया है और उसकी आसक्ति अब मुझमें है, अतः मुझे विलम्ब नहीं करना चाहिए।' ऐसी प्रतीति होने पर वह आध्यात्मिक उन्मीलन एवं उच्चतम तत्त्व के प्राप्त्यर्थ सब अनिवार्य साधन उस साधक को प्रदान करता है जिसे वस्तुतः उसकी आवश्यकता हो, जो केवल उसे और उसे ही चाहता हो और अपने अन्वेषण में अनन्यासक्त हो। अतएव उत्कण्ठा, तीव्र अभिलाषा करना तो हमारा कर्तव्य है। सीमित बुद्धि वाले मनुष्य को यह पग उठाना है और यदि वह विशुद्ध एवं निष्कपट है, तो उसकी पूर्ति का भार प्रभु पर है। महापुरुष ईसामसीह ने कहा था- "तुम माँगो और तुम्हें प्राप्ति हो जायेगी।" इसकी याचना करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है और बोध-मिश्रित प्रेम द्वारा पूर्ति करना ही निश्चयेन उस पिता का कर्तव्य है और वह इतना ही निश्चित है जितना रात्रि के अन्धकार को गरिमामय प्रभात और दीप्तिमान् अदिति का अनुसरण करना है।
परमात्मा के लिए सत्यान्वेषी की सत्याकांक्षा की पूर्ति, रात्रि की कालिमा का अनुसरण करने वाले लालिम प्रभात और दीप्तिमान् अदिति के अनुसरण की भाँति सुनिश्चित है। प्रार्थना, उपासना एवं ध्यान के यह अवसर हमारे जीवन में प्रभु-कृपा की स्पृश्य-विद्यमानता के ही प्रमाण नहीं, प्रत्युत् हमारी ओर से उसके लिए हमारी उत्कट कामना का भी प्रमाण है। जब भी हम भौतिक पदार्थों से विमुख होते हैं, प्रत्येक बार जब भी संसार की वस्तुओं को त्याग कर अन्तरंग की प्रशान्ति में स्वयं को समाहित करके उसकी उपासना के लिए आसीनस्थ होते हैं, एक पुकार उस अनन्त की ओर जाती है-"मैं यहाँ हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। कृपा करो। अपना दर्शन दो। मैं नश्वर संसार से विमुख हो कर शाश्वत की आकांक्षा करता हूँ।" यह अन्तर्मन जीव की उत्कट इच्छा, आत्मा की विलक्षणता और उत्कण्ठा का मानो चिह्न स्वरूप बन जाता है।
ध्यान का रूप और योग में इसका स्थान
अतः ध्यान आपकी सत्ता के गहनतम भाव की क्रिया है। वस्तुतः यह मानव-जीवन के विशिष्टाधिकार, परम आनन्द की सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट क्रिया है। इस भूतल पर उपासना से महत्तर कोई भी क्रिया नहीं है। शान्ति में प्रवेश करते हुए उस प्रभु की विद्यमानता के अलौकिक तेज में स्नान करते हुए इस रमणीय प्रभात वेला; पुण्य क्षण एवं दिव्य सन्निधि की वेदी पर आसीनता की सौभाग्य-प्राप्ति हेतु हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे भीतर जो-कुछ पार्थिव तत्त्व है, उससे निवृत्त होने, स्वयं को पवित्र करने तथा दिव्य तत्त्व से परिपूर्ण करने का हमें जो यह सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए हमें प्रभु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ध्यान की ये क्रियाएँ उस प्रक्रिया के अवान्तर रूप हैं जिसके प्रति हमारा सारा जीवन उद्दिष्ट है। परमेश्वर के समक्ष सतत अपने हृदय-पट को खुला रखना ही हमारे जीवन का ध्येय है-जो स्व प्रकृति की शान्ति का क्रम है, अनात्मा के बोध से विमुख होने का सतत क्रम है, हमारे अस्तित्व के ऊपर अनित्य की पुकार की उपेक्षा का क्रम है, अविनाशी शाश्वत आत्मा के समक्ष स्वयं के तत्काल उन्मीलन का दृढ़ संकल्प, दृढ़ आग्रह है। हमारे समस्त जीवन का लक्ष्य असत्य से विमुख होना एवं सत्य के प्रति उन्मुख होना है। यह अन्धकार के कर्षण का बहिष्कार तथा ज्योति, केवल ज्योति की आकांक्षा का प्रयास है; इस मृत्युलोक से ऊपर उठ कर आभ्यन्तर आत्मा की नित्य प्रकृति के अभिज्ञान की धारणा है तथा ध्यान उसी प्रक्रिया का गहन, सुबद्ध तथा विचारपूर्ण ढंग से निष्पन्न घनीभूत रूप है जो एक विशिष्ट समय पर एक विशिष्ट दिशा में प्रवाहित होता है। ध्यान आत्मा में नितान्त स्थिति का नाम है और हमारा सम्पूर्ण जीवन (तथा इसकी गतिविधियाँ) ध्यान-तत्त्व के उत्साह का तथा आध्यात्मिक गवेषणा के उल्लास का विकीर्ण प्रवाह है। अत: इन दो क्रमों में इन्हें परस्पर पृथक् करने वाली कोई रुकावट अथवा विघ्न नहीं आने देना चाहिए। ध्यान हमारे प्राणों का आधार बनना चाहिए। ध्यान गहन रूप से हमारी जीवन-ज्योति को पुनः गतिशील करने का साधन होना चाहिए। ध्यान हमारे सम्पूर्ण जीवन, समस्त विचारधारा, भाव, आचार-विचार, संकल्प एवं आकांक्षाओं तथा विश्व के साथ हमारे व्यवहार की प्राण-संचारक शक्ति होनी चाहिए। सम्पूर्ण संसार और जीवन के प्रति हमारा बोध ध्यान की आन्तरिक प्रेरणा से गतिमान होना चाहिए। जीवन और ध्यान दोनों सतत एवं संलग्न प्रक्रियाएँ हैं। एक-दूसरे को स्पष्ट रूप से वियुक्त करती हुई वे दो प्रक्रियाएँ नहीं हैं।
ध्यान कोई ऐसी विश्लिष्ट क्रिया नहीं है जिसका आप अनुष्ठान करें और जीवन में उसका अवस्थान न हो अथवा सर्वथा भिन्न स्वभाव की हो और जो आपकी सामान्य जीवन-धारा के विपरीत हो। तथापि यह सम्भव है कि यह आपकी निम्न प्रकृति के, मन की इच्छाओं और इन्द्रियों की विषयोन्मुखता की सामान्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हो। इस प्रकार की बहिर्मुखी क्रियाएँ मन की आन्तरिक प्रवृत्तियाँ हैं और ध्यान इनके विरुद्ध जा सकता है; परन्तु बाह्य क्रियाएँ आपकी 'आत्मा' नहीं, इन्द्रियाँ आपकी आत्मा नहीं, मन और आकांक्षित प्रवृत्ति आपकी आत्मा नहीं। आपका वास्तविक स्वरूप सागर की ओर अभिसृत नदी के समान है। एवंविध, वस्तुतः आपके जीवन और ध्यान में असमानता नहीं होनी चाहिए।
यदि मन में यह धारणा न हो तो आप अनुभव करेंगे कि आपके दैनिक जीवन और ध्यान में एक स्पष्ट भ्रान्ति है और आपके दैनिक जीवन से उद्भूत प्रवृत्तियों और ध्यान में एक संघर्ष-सा होने लगता है। यह एक कठिन प्रक्रिया हो जाती है जिसमें मन का एक पक्ष दूसरे का विरोध करता है, प्रतिषेध करता है जिससे सारभूत शक्ति का हास होता है। जीवात्मा के अन्तस्थल में संघर्ष होने लगता है। जिस समन्वय, शान्ति और उल्लास से, ध्यान के द्वारा आपका अस्तित्व प्रफुल्लित हो सकता है और आपकी मुखमुद्रा, अन्तःस्थिति सन्तोषप्रद हो सकती है, आपकी अभिव्यक्ति में उसका अभाव है; आप ध्यानस्थ होते हैं, किन्तु आपकी दृष्टि में शान्ति नहीं है, जहाँ इस आन्तरिक रहस्य का अभिज्ञान होता जाता है, जीवन और ध्यान का क्रम साथ-साथ चलने लगता है, दोनों ही एक स्वर-ताल में बद्ध रहते हैं; तब मानो ध्यान की स्थिरता ध्यानयोगी के जीवन में आप्लावित हो उठती है; उसके नेत्र ध्यानमय शान्ति के तेज से प्रकाशित हो उठते हैं; उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व ध्यान की प्रसन्नता से स्पन्दित और देदीप्यमान हो उठता है। वस्तुतः आपके जीवन में ध्यान का यही स्थान है। आपके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की दिनचर्या में वस्तुतः ध्यान की यही भूमिका है।
ध्यान की प्रक्रिया प्रारम्भ कैसे की जाये-समुचित विधि
हम सदेह प्राणी हैं और हमारा मन भी जिस प्रकार का है, हमारी दिनचर्या का, हमारे आत्म-चैतन्य, अन्तस्तम जागरूकता पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है और हमारी इन्द्रियाँ आभ्यन्तर चेतना की प्रभा को पुनः-पुनः आच्छादित करती हैं। अतएव, ध्यान के लिए आसनस्थ होते ही तत्काल प्रक्रिया प्रारम्भ न कीजिए। बाह्य जीवन के संवेग को शान्त करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। थोड़ा-सा समय दो। विचारों को शान्त होने दो। जब मन की चंचलता का भँवर शान्त हो जाये, मन स्थिर हो जाये, तब इसे स्व-जागृति से शनैः-शनैः ऊपर उठाओ। मन को इसके तात्कालिक सम्पर्कों एवं देह के साथ संयोग की चेतना से बाहर ले आओ। तब तक दिव्य नाम, दिव्य मन्त्रों का उच्चारण करो। इस मन्त्रोच्चारण से अद्भुत आध्यात्मिक तरंगों का प्रादुर्भाव होता है जो दिव्य शक्ति सम्पन्न होती हैं और परमात्मा की दिव्य सूक्ष्मतम जागृतावस्था तक पहुँचने के लिए मन की सहायक होती हैं। मन के संहरण की निश्चलता से प्राप्त प्रशान्ति और उत्थान की अवस्था में दिव्य नाम परमात्मा के प्रति आपके भाव को, परम सत्य के प्रति आपकी विचारधारा को प्रबुद्ध करता है। समस्त देह, सम्पूर्ण मन और इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं; मन उन्नत हो जाता है। उन्नत संकल्प पर ध्यानस्थ होने के लिए अब यह उद्यत है। शनैः शनैः मन के अधम भावों से आसक्ति क्षीण होने लगती है। अतः दिव्य भाव से, एक प्रकार के आध्यात्मिक प्रेम से मन को आपूरित करके मन को ध्यान के लिए तैयार करना चाहिए। यह कुछ इस प्रकार है : पर्वतों और घाटियों, वन और रमणीय दृश्यों के विस्तृत प्रदेश से यात्रा कर लेने के उपरान्त आप अकस्मात् ही सागर-तट पर पहुँचते हैं। उस समय के सभी विविध नाम और रूप तथा सदा परिवर्तनशील विषय उपरान्त हो जाते हैं और आप केवल एक विशाल विस्तरण को देखने लगते हैं। आपकी दृष्टि किसी भी बाह्य पदार्थ से पूर्णतया अविचलित है। आप केवल विशालता का, केवल स्थिरता का आलोक करते हैं। आप अनेकता से एकता की दृष्टि प्राप्त करते हैं।
मनोनिग्रह, आत्म-संहरण, आत्म-स्थिरता मन्त्रों के द्वारा एवं स्तोत्र-गान के द्वारा आत्म-चैतन्य के उत्थान की ये प्रक्रियाएँ आपको ऐसी अवस्था में ले जाती हैं, जहाँ मन सब विविध विषयों (की आसक्ति) से मुक्त हो जाता है और केवल उसी अन्तर्वासी ईश्वर परब्रह्म परमात्मा, सत्यस्वरूप, परम सत्य, परम तत्त्व, अव्यय, असीम पर ही केन्द्रित हो जाता है। जिस प्रकार पूर्वी सागर के सुदूर क्षितिज से उदय होता हुआ सूर्य-वृत अनिर्वचनीय विशालता में आ जाता है, उसी प्रकार उस पवित्र तत्त्व परमात्मा-रूपी सागर के प्रति आपका बोध भी उसी विशालता को प्राप्त करता है।
इसका स्वरूप किसी ध्वनि, दिव्य व्यक्तित्व, निराकार, विचार-विशेष अथवा परमात्मा के सम्बन्ध में आपके विचार-समुदाय के रूप में प्रकट हो सकता है मानो स्वयं सागर ही अपने से अभिन्न, अपने से अपृथक् तद्रूप होते हुए भी काल-विशेष में ऊर्मीजाल-सा प्रतीत होता हुआ लहर के रूप में परिवर्तित हो गया हो। आप शुद्ध तत्त्व-रूपी सागर का भगवान् के प्रति अपने एक विचार-विशेष के आलोक का, अपने विचार अथवा विचार-श्रृंखला के रूप में आह्वान करते हैं और शनैः शनैः सहज रूप से उस विचार-समुदाय अथवा व्यक्तित्व की ओर अग्रसर होते हैं। आपकी समग्र सत्ता प्रेम, उपासना, पूजा-भाव, प्रार्थनापरता और निष्ठा की सतत प्रवाहिनी धारा के रूप में पिघल कर तब तक प्रवाहित हो, जब तक कि आपका समस्त व्यक्तित्व दिव्य भावनाओं से परिपूर्ण सतत स्रावित स्रोत की भाँति प्रतीत न हो जो आपके ईश्वरीय भाव की ओर निःशब्द हो कर प्रवाहित हो रहा है।
इस स्वरूप को सतत, अटूट, प्रेममय भगवत्-चिन्तन में स्थायी रखने का प्रयास करना चाहिए। यही ध्यान का नितान्त सार है। यह मन की ऐसी अवस्था है, जब सम्पूर्ण मन भगवान् और केवल भगवान् से ही परिपूर्ण होता है- भगवान् के अतिरिक्त अन्यथा किंचिदपि दृष्टिगत नहीं होता। ऐसी अवस्था में ध्यान की प्रक्रिया का अभिज्ञान नितान्त आवश्यक है। ध्यान के विषय में अनेक मिथ्या मत, मिथ्या विचार प्रचलित हैं जिनमें से एक यह है कि ध्यान मन को रिक्त करने का प्रयास है। इस मत के समक्ष आने पर मुझे यह उक्ति स्मरण हो आती है- "खाली मन, शैतान का घर।" मन खाली हो, तो कोई भी विचार प्रवेश कर सकता है। जनगण के हृदयों से सम्बन्ध विच्छेद अत्यन्त कठिन है; क्योंकि इसमें अंशतः सत्य निहित है। आप पूर्ण असत्य का विरोध कर सकते हैं; किन्तु असत्य यदि अंश-रूप में है, तो उसमें सत्य भी अंश-रूप में निहित होता है और इसका विरोध करना दुष्कर हो जाता है। अंशतः असत्य (आधा झूठ) बोलना पूर्ण से कहीं अधिक भयंकर है। अतः ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया की पूर्णतया उपेक्षा करने वाले तथा इसे अंशतः ग्रहण करने वाले लोगों से मैं कहा करता हूँ- "मन को भगवद्भाव से परिपूर्ण करना ध्यान है।'' इसका अभिप्राय है-ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सर्व विचारों से मन को शून्य रखना। अनात्मक अथवा अदिव्य तत्त्वों का मन से निराकरण प्रक्रिया का एक अंश है। वास्तविक प्रक्रिया में केवल वस्तु की ही उपलक्षणा होती है। ईश्वर (भाव) से मन को पूर्ण करना (मन में ईश्वर को अधिष्ठित करना) ही वास्तविक प्रक्रिया है। वहाँ जागृति सदैव विद्यमान है। मन को रिक्त करने पर शून्यता अथवा रिक्तता का सृजन नहीं होता, प्रत्युत् ईश्वर इसे भरता है। परब्रह्म अनन्य सत्य सत्त्व शुद्ध सत्ता की ज्योति आपकी चेतना के सम्पूर्ण क्षेत्र में आप्लावित हो उठती है। उसे भगवान् पूर्ण करता है और जहाँ 'वह' है वहाँ संसार नहीं रह सकता। उक्ति है- “जहाँ परब्रह्म परमेश्वर का वास हो, वहाँ जगत् की इच्छा नहीं रहती।" अतः जहाँ भगवान् ने आना है, वहाँ जगत् की इच्छा नहीं होनी चाहिए; क्योंकि जगत् के साथ भगवान् नहीं रह सकता। भगवान् कहता है- "मैं ईर्ष्यालु स्वामी हूँ। ममार्थ जो स्थान बना है, उसमें मैं किसी अन्य की विद्यमानता स्वीकार नहीं करूँगा। यह मेरा अवस्थान है।" मानव-हृदय भगवान् का राजकीय अनुपम सिंहासन है। अन्य किसी पदार्थ की विद्यमानता को देख कर वह कहता है-"नहीं, यह मेरे आगमनार्थ तैयार नहीं है।"
अतः ईश्वर व्यतिरिक्त तत्त्व का आभ्यन्तर से निराकरण करके उसे ईश्वर से परिपूर्ण करना ही ध्यान है। दिव्य स्वरूप परमात्मा के लिए एक मत-विशेष बनाना कोई महत्त्व नहीं रखता। सबसे बड़ा अभिशाप वह है जो परमात्मा के प्रति एक मत अथवा धर्म-विशेष का प्रतिदान करके उसे मानवता पर थोप देते हैं कि और इस बात पर बल देते हैं कि भगवान् इस-इस प्रकार का है और आप अमुक पुस्तक द्वारा अथवा अमुक विधि से ही उसका चिन्तन करें। ऐसा कहना भगवान् के प्रति पावन धारणा का तथा आभ्यन्तर आध्यात्मिक तत्त्व का विनाश करना है। भगवान् की परिभाषा नहीं दी जा सकती। वह बोधातीत है। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते; किन्तु वह प्रेम-स्वरूप है। किसी भी विधि से उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। एक शिशु जैसे अपनी माँ के बाल खींचता है, उसकी नासिका घुमा देता है, उस पर चपेट-प्रहार करता है, उसका मुख घुमाता और खींचता है अथवा अपनी उँगलिका उसकी आँख में डालता है या कुछ भी करने पर माँ बच्चे को प्यार करती है। शिशु बाल खींचता है, तो वह झुक जाती है। बालक की इच्छा के अनुसार अपना चेहरा घुमाती है। क्यों? प्रेम के कारण! माँ का शिशु के प्रति और शिशु का माँ के प्रति प्रेम! इस प्रकार प्रेमार्द्र हृदय भगवान् की यथाशक्ति जिस-किसी भी रूप में कल्पना करता है, वही भगवान् है। भगवान् कहते है-"सत्यान्वेषी जिस रूप में मेरा ध्यान करते हैं, मैं उसी रूप में उन्हें दर्शन देता हूँ।" और यदि आप 'उसे' अपनी कल्पना में निबद्ध करने का प्रयास करेंगे तो आप ईश्वर के असीमित, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी आदि रूपों का संहार ही करेंगे। वह क्या नहीं कर सकता? वह क्या नहीं है? वह सर्वस्व है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो उससे व्याप्त नहीं। अतएव, यद्यपि हम जानते हैं कि वह सम्पूर्ण है, सर्वातिरिक्त है, सब नाम और रूपों से परे है, मन और कल्पना से परे है, तथापि वह सर्वस्व है। वह सर्वातिशायी है।
परब्रह्म को किसी भी प्रकार का बोधगम्य रूप देने के प्रयासों में वेदान्त को महान् पराकाष्ठा प्राप्त है। वेदान्त की उक्ति है-"अनेक नाम और रूपों वाले तुम सर्वस्व हो, तुम असीम हो !" अतः किसी भी रूप में आप उसकी कल्पना करें। विचलित न हों। उत्सुक भी न हों; क्योंकि आप जब ध्यानस्थ होते हैं, तो परमेश्वर को सब ज्ञान रहता है। उसे सर्वविदित है। वह यह भी जानता है कि आप बैठे कहाँ हैं। ध्यान में विचारमग्न होने पर परमात्मा आपके उस विचार को भी जानता है।
परिवार के पिता को ही लीजिए। वह एक सज्जन है, सबके स्नेह का पात्र है और कल्पना कीजिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का उससे पृथक् सम्बन्ध है। पुत्र और पुत्री उसे पिता की दृष्टि से देखते हैं, कोई आदर और वृद्ध की दृष्टि से देखते हैं- जो उनका पालन-पोषण एवं रक्षण कर रहा है और अनुसरण करने योग्य व्यक्ति है। उसका भाई उसे पिता नहीं वरंच अनुग्राही भ्राता की दृष्टि से उसका अवलोकन करता है। पत्नी के लिए वह स्वामी, भगवान् और प्रेमी पति है। उसके अपने माता-पिता उसे अपना पुत्र, अपने पोतों का पिता मानते हैं। उसका प्रतिवासी (पड़ोसी) उसके प्रति इन सबसे सर्वथा भिन्न धारणा रखेगा। माता-पिता, बच्चे, भ्राता, पत्नी और प्रतिवासी के मन की अवधारणाएँ पृथक् पृथक् हैं। एक ही व्यक्ति के लिए उन सबके हृदयों में विविध विचारधाराएँ हैं; किन्तु वे न्याययुक्त और उचित हैं।
मन को ब्रह्म-विचार से आपूरित करो
आपका हृदय जैसी भी उसकी कल्पना करे, उसी प्रकार से आपको भगवत्-चिन्तन करना चाहिए। इस प्रार्थना से दैनिक कार्यक्रम प्रारम्भ कीजिए-"हे प्रभु! मैं इस वेदी पर आपके समक्ष प्रेम का उपहार ले कर आया हूँ। मैं नम्र भाव से आत्म-समर्पण करता हूँ। मैं स्नेह से आया हूँ। मेरी चेतना का अपनी महान् दिव्य प्रकृति की वेदी पर आरोहण करो। मेरे उत्थान हेतु आप प्रसन्न हो जाओ। इन्द्रियाँ और मन शान्त हो जायें। महारव न करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य वेला में वे अनाहूत प्रवेश न करें। मैं आपका, केवल आपका ही चिन्तन करता हूँ। मैं पूर्ण समग्र रूप से आपमें विलीन होना चाहता हूँ।" इस प्रार्थना के उपरान्त ही प्रभु पर ध्यान प्रारम्भ कीजिए। यदि अन्य विचार मानस पटल पर उतरते हैं, तो भी उनकी उपेक्षा कीजिए। मन के प्रति बोध-शून्य रहें। इतना ही कहें- "मैं तो अपने प्रभु का ही चिन्तन करूँगा। तुम्हारी जो इच्छा हो करो। मैं तो अपने प्रिय का ही ध्यान करूँगा। तुम्हारे साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।"
मन का दमन करने का प्रयास न करें। वृत्तियों का बलपूर्वक निराकरण न करें। बल का प्रयोग न करें, अन्यथा आपके लक्ष्य प्रभु-चिन्तन में बाधा पड़ेगी और आप मन का चिन्तन करने लगेंगे। आपकी वृत्ति प्रभु पर एकाग्रित होने की अपेक्षा आक्षिप्त हो उठेगी और निषेधात्मक प्रक्रिया में इसका अस्थाने असत्प्रयोग होगा। निषेधार्थक प्रक्रिया में आपको अपनी शक्ति का हास नहीं करना चाहिए। विचारों का ध्यान न करें। मन की चिन्ता न करें। इनकी उपेक्षा करके हृदय-ग्रन्थि को परमात्मा से सन्निबद्ध कर लें। यदि मन दिव्य तत्त्व से विमुख होने लगे, तो 'ॐ ॐ ॐ ॐ...' का उच्चारण करें और अनन्त, असीम, शाश्वत, सर्वोत्तम (सर्वान्तर्यामी) परमात्मा के विचारों से मन को परिपूरित करें। अथवा, अपने इष्ट का स्मरण करें। एवंविध, मन को भौतिक विचारों से सर्वथा स्वच्छ करके केवल भगवान् का चिन्तन करें। अब भगवान् का नाम पुनः पुनः उचारें और भगवान् से सम्भाषण करते हुए यह प्रार्थना अर्पित करें-"मेरे प्रभु, आप सर्वस्व हैं, अपने अस्तित्व का, अपने हृदय का समग्र प्रेम आपके चरणों में समर्पित करता हूँ।" अभिप्राय केवल इतना ही है कि आप अन्य सब कार्यों को विस्मृत करके ब्रह्म-विचार, सौन्दर्य, प्रकाश, ज्योति, दिव्य संकल्प, परमात्मा की विद्यमानता और उसकी सन्निधि का आभास अनुभव करें। यह प्रक्रिया करते समय प्रत्येक क्षण, आपकी चेतना की गहराई में एक रूपान्तरित प्रक्रिया का उदय होता है। आत्मा की अधिकाधिक ज्योति आपके समस्त अस्तित्व को पूर्ण करने लगती है। जब आप परमात्मा में पूर्णतया विलीन हो कर ऐसे भाव से युक्त होते हैं, तब वस्तुतः आप परमात्मा के देश में प्रविष्ट हो जाते हैं। उस क्षण के लिए आपकी सम्पूर्ण सत्ता प्रभु-सत्ता में रूपान्तरित हो जाती है और ध्यान से बाहर आने पर यह भगवद्-प्राप्ति का प्रभाव जिसका आपने सृजन किया था, वह पर्यवस्थित रहता है।
अखण्ड रूप से, प्रतिदिन पुनः पुनः ऐसा करने से दिव्य स्वरूप का भाव आपकी चेतना का अटूट अंग बन जाता है और आप सर्वदा दिव्य स्वरूप से अनन्यानुभूति करने लगते हैं। आप अनुभव करते हैं- "मैं यह शरीर नहीं हूँ। मैं यह मन नहीं हूँ, इन्द्रिय नहीं और बुद्धि भी नहीं हूँ। मैं परमात्मा के शाश्वत सूर्य का अंश हूँ। उसके प्रतिबिम्ब से बना हूँ। उसके साथ एकरूप हूँ। अन्तःस्थित महान् तेजस्वी प्रकाश की देदीप्यमान रश्मि हूँ।" भावों के जिस आधार पर मन आधारित रहता है, अत्यन्त विनीत भाव से, प्रेम से अन्तस्तम में एकत्र समग्रता और एकाग्रता से मन वही रूप धारण कर लेता है।
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको मन की अद्भुत एकाग्रता और गहन ध्यान में सफलता का आशीर्वाद दें!
४. सच्चा वैराग्य
भगवान् की आनन्दमयी सन्तान! शाश्वत दिव्य ज्योति की देदीप्यमान रश्मियो। प्रणाम! गुरुदेव शिवानन्द और हिमालय की पावन भूमि, गंगा तथा उपनिषदों एवं वेदों की पवित्र धरती के साहित्यिकी कोष से आपके लिए अत्यन्त हर्षोल्लास के साथ एक छोटा-सा सन्देश ले कर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ।
सब देशों में सदा, विश्व के प्रत्येक भाग के जन-समूह के लिए भारत माता आध्यात्मिक ज्योति के महान् ज्योति-पुंज का अवस्थान रही है। आत्म-साक्षात्कार, भगवद्-साक्षात्कार के महान् उद्देश्य को उसने सदा सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। भारत माँ की सन्तान को सदा से ही भगवद्-प्राप्ति की महती जिज्ञासा रही है। बाह्य दृष्टिगोचर लोक के सब पदार्थों की अपेक्षा परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष और दिव्य साक्षात्कार में कहीं अधिक आनन्द पाया है।
वैराग्य विवेक पर आधारित हो
वैराग्य भारत के महर्षियों के उपदेश का सार रहा है। वैराग्य में आध्यात्मिकता का सार और भगवद्-साक्षात्कार का रहस्य निहित है। तन्द्रा, पलायन अथवा उत्तरदायित्व का उत्सर्ग वैराग्य नहीं है। स्वर्लोक के साम्राज्य की ओर यात्रा में साधक को इससे महान् शक्ति प्राप्त होती है। परब्रह्म की विकट यात्रा में साधक को संन्यास का बल ही धैर्य प्रदान करता है।
इन्द्रिय-सुख की आकांक्षाओं का परित्याग शाश्वत सुख का द्वार है। योग के साधकों तथा आध्यात्मिक पथ के सत्यान्वेषियों के लिए सभी योग्यताओं में वैराग्य का स्थान सर्वोच्च है। वैराग्य ही आपको निर्भय और सुखी बना सकता है। वह प्रशान्ति की वृष्टि करके अन्ततः अमरत्व प्रदान करता है।
इस ब्रह्माण्ड की प्रकृति के गर्भ में प्रवेश करके तथा इस तथ्य का अनुमान लगा कर कि सब नाम और रूप दोषपूर्ण हैं, अस्थायी हैं, परिवर्तनशील हैं और नश्वर हैं, मनुष्य को सुबोध, विवेक तथा गवेषणा द्वारा इस संसार से उद्विग्न हो जाना चाहिए। एवंविध विलासपूर्ण जीवन के दोष देख कर मनुष्य को वास्तविक वैराग्य हो जाता है।
संसार से उद्वग्नि होने का अभिप्राय सांसारिकता से उद्वेग है। भौतिक विषयों से उद्विग्न होने की अपेक्षा हमें विषय-प्राप्ति की इच्छा, उसके अध्यासन (अधीनता) से उदासीन होना चाहिए। विवेक हमारे वैराग्य को बल देने वाला होना चाहिए। वैराग्य विवेक-शक्ति पर आधारित हो, तो चिरस्थायी होता है; क्योंकि इसका आधार दृढ़ है। क्षणिक भावुक उथल-पुथल के परिणाम स्वरूप वैराग्य नहीं होता। पत्नी, पदवी, मित्र, पुत्र, सम्पत्ति आदि के वियोग से जो क्षणिक वैराग्य जागृत होता है, वह अधिक सहायी नहीं होता। वह तो एक प्रकार की क्षणिक लपक मात्र है। ऐसा वैराग्य स्थिर नहीं हो सकता। यह तो गवेषणा, विवेक अथवा निरन्तर स्वाध्याय से जागृत हो सकता है।
वैराग्य की आवश्यकता का विश्वास ज्ञान-शक्ति, गवेषणा और विवेक के बिना उदित नहीं होता। क्षण-भर के लिए मानव की नियति पर ध्यान दें। शिशु-रूप में मनुष्य गर्भ में मूत्र, पस और मल से अवगुण्ठित रहता है और क्षुधाग्नि से सन्तप्त होता है। प्रौढ़ होने पर इन्द्रिय-भोग तथा आसक्तियों में फूला नहीं समाता। वृद्ध होने पर शरीर और बुद्धि अत्यन्त शिथिल हो जाते हैं और तब अपने सम्बन्धी भी उपेक्षा करने लगते हैं। ऐसे पुरुष से कोई सम्बन्ध भी नहीं रखना चाहता।
भौतिक जीवन की निःसारता
भोग-विलास, धन-वैभव तथा ऐन्द्रिक विषयों में आसक्त जीवन सर्वसामान्य पुरुष का दुःखद भाग्य है। जीवन क्षणभंगुर है। विषाक्त सर्प की भाँति फण फैलाये हुए मृत्यु सर्वदा आक्रमण करने को उद्यत चुपके से आपकी ओर अग्रसर हो रही है। विविध गम्भीर रोग शरीर को छिन्न-भिन्न कर देते हैं। यौवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और वृद्धावस्था शरीर को आ घेरती है। परमार्थ की प्राप्ति हेतु विवेक, वैराग्य और गवेषणा द्वारा अमोघ जीवन का सद्यः सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही सुरक्षित रहता है। ईश्वर की प्रवचंक शक्ति माया एक महान् मणिकार है। वह पिंजर तैयार करके उसे त्वचा और नाड़ी से आवृत करती है तथा विभिन्न अशुद्धियों को अत्यन्त सुन्दर ढंग से भीतर ही छिपा देती है। अहा! तत्काल ही मनुष्य माया-विरचित इस गुड़िया के रूप पर पूर्ण रूप से मोहित हो उठता है। इस देह को आप कब तक माया कहते रहेंगे? अभ्रान्त कल्पना को पुष्ट करें तथा स्वयं को वास्तविक प्रकृति सच्चिदानन्द से तद्रूप करें जो आपका वास्तविक स्वरूप है।
क्या आप यह कहते-कहते थके नहीं-"मेरा पुत्र टाइफाइड से ग्रस्त है। मेरी दूसरी पुत्री का विवाह हो रहा है। मेरी पत्नी नयी पोशाक लेने के लिए मुझे व्याकुल कर रही है। मेरा पति शराब और जुए के दुर्व्यसन में पड़ गया है। मेरे पौत्र का स्वर्गवास हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ।" वस्तुतः जीवन के महान् लक्ष्य के प्रति आपके नेत्र इन कष्टों से खुल जाने चाहिए। वैयक्तिक प्रेम खोखला है। यह पाशविक आकर्षण है। यह केवल राग है। यह आधिभौतिक प्रेम है। यह ऐसा प्रेम है जो पूर्णतः स्वार्थपरक है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी सुख की आशा में ही प्रेम करता है। इसका आधार स्वार्थ है और यह सदा परिवर्तनशील है। एक व्यक्ति का अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम अन्यान्य बाह्य तत्त्वों पर आधारित होता है जो अस्थिर हैं। उनमें परिवर्तन आने पर मनुष्य की भावुक वृत्ति भी परिवर्तित होती है। मुख्यतः, यह दिखावा है। प्रिय मित्र! सत्य, शाश्वत प्रेम तो तुम्हें केवल परमात्मा में अथवा सन्तों में प्राप्त हो सकता है। केवल परमात्मा ही प्रेम करना जानता है। उसके प्रेम में विकार नहीं आता, न्यूनता नहीं आती।
प्रिय मित्र! मुझे बताओ, तुम कब तक संसार के इन क्षणिक पदार्थों के दास बने रहना चाहते हो? क्षणभंगुर इन्द्रिय-सुख का पुनरावर्तन कब तक करोगे? दिन-प्रतिदिन, प्रातः मध्याह्न, सायं-रात्रि? इस देह की, इन भोग-विलासों की कब तक पूजा करना चाहते हो? इन अनित्य क्षणिक पदार्थों का मोह-रूपी बन्धन तोड़ कर, सब इच्छाओं, तृष्णाओं तथा राग से विरक्त हो कर भगवान् पर ध्यान लगाने और जीवन में धर्म-कार्य करने का समय आपको कब मिलेगा? विचार करो! चिन्तन करो! क्या वास्तव में ही इस संसार में कोई सुख-सन्तोष है? सोचो, विचारो, नित्य चिन्तन करो! लौकिक विषयों की प्रकृति का विश्लेषण करो। उनकी प्रकृति और उनसे प्राप्त अनुभवों के स्वभाव की गवेषणा करने का प्रयास करो। देखो! वे कितने अपूर्ण हैं, कितने असमर्थ हैं, कितने श्रम, व्याकुलता, इच्छा, कामना और निराशा के अंशों से व्याप्त हैं। इन इन्द्रिय-सुखों की प्राप्ति हेतु कितने असत् विचार एवं असत् कार्य अनिवार्य हैं। गली के एक कुत्ते की भाँति अस्थियों की खोज में मनुष्य क्यों इस भूलोक के नश्वर पदार्थों से प्राप्त अल्प एवं तुच्छ सुखों के लिए आलस्यपूर्ण विचरण करता है? इन वस्तुओं के मोह का पाश तोड़ डालो। भीतर खोजो। अन्तरावलोकन करो। शान्ति और अमृतत्व के परम धाम का अन्तर्दर्शन करो। उसका साक्षात्कार करो।
विलम्ब मत करो। विरक्त हो जाओ। वैराग्य की महिमा को पहचानो। काया-क्लेशों की गुरुता, इन्द्रिय-सुखों की नितान्त निरर्थकता एवं परमात्मा की प्राप्ति और इस प्राप्ति हेतु वैराग्य की महती आवश्यकता का ज्ञान करो।
लौकिक वृत्ति वाले उन्मादक जनों की ओर से विमुख हो जाओ। ईश्वर में आस्था दृढ़ करो और पवित्र विचार, उच्च आदर्श एवं परमज्ञानमय जीवन व्यतीत करो। सार्वभौमिक प्रेम, सत्य एवं पवित्रता को जीवन में पथ-प्रदर्शक सितारों के रूप में अंगीकार करो। असत्य का परित्याग करो। स्वभाव की कर्कशता त्यागो। अशुद्धता त्यागो। पथ-विचलित होने अथवा पृष्ठावलोकन से इनकार करो। यथासमय आपको साक्षात्कार अवश्य होगा।
अनिवार्य साधनाभ्यास द्वारा वैराग्य जागृत करो। इन सबका उद्देश्य दमन एवं शमन तथा आपको वैराग्य में स्थिर करना है। मन की चपलता को संयत करना चाहिए। हृदय सार्वभौम प्रकाश और प्रेम के परम आदर्श में संलग्न हैं। यथासम्भव स्वामी शिवानन्द के बीस आध्यात्मिक नियमों का नम्रता और श्रद्धा के साथ प्रतिदिन अनुशीलन करो। जितना अधिक आप इसमें सफल होंगे, उतनी ही अधिक आपको मानसिक शान्ति और शक्ति प्राप्त होगी। आपकी शारीरिक अवस्था पर भी इसकी प्रतिक्रिया अच्छी होगी और शनैः शनैः आप शक्ति और वैराग्य में समृद्ध होंगे।
मन में तीन तत्त्व ऐसे हैं जो आन्तरिक परम सत्ता के आलोक में विघ्न डालते हैं। प्रथम तत्त्व है आपकी निजी प्रकृति की बाह्य अशुद्धता - अनेक इच्छाएँ, आकांक्षाएँ, तृष्णाएँ, अनुराग, रुचि, अरुचि आदि। द्वितीय है-मन की अनियन्त्रित चपलता। संयत मन चिन्तित नहीं होगा। मन की चंचल प्रवृत्ति ही अशान्ति और चिन्ता का कारण है और यह अशान्ति इच्छाओं और कामनाओं के कारण होती है। अतीत सुख, अनुभव एवं कर्मों के कारण मन अंकित गुप्त संस्कारों की अशुद्धताएँ ही आपकी अशान्ति और चिन्ता के लिए उत्तरदायी हैं। तृतीय बाधा का मूल भी यही (इच्छा) है। क्रोध तथा उत्तेजना इच्छा से उत्पन्न होते हैं और क्रुद्ध होने पर, उत्तेजित होने पर आप अशान्त होते हैं और विवेक खो बैठते हैं। इच्छा को वशीभूत करना है और मन को शान्त करना है।
आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन, निःस्वार्थ-भाव का संवर्धन तथा सक्रिय सेवा-भाव, दान, प्रार्थना एवं पूजा-रूप में प्रभु-भक्ति और दिव्य नाम के जप अथवा विविध संकीर्तन द्वारा सदा श्रद्धापूर्वक भगवद्-स्वरूप से व्यक्तित्व की इन शारीरिक और मानसिक अशुद्धताओं का निराकरण करना चाहिए। आपके बाह्य व्यक्तित्व की अपूर्णताओं के लिए भगवान् का नाम अत्यन्त शक्तिशाली है। दिव्य जीवन व्यतीत करने से ही आप अपनी दैहिक एवं मानसिक प्रकृति की अपूर्णताओं पर विजय पा सकोगे और निःस्पृहा तथा वैराग्य में आनन्द लोगे।
जीवन की पहेली
जीवन और ब्रह्माण्ड दोनों की निगूढ़ पहेली को समझने का प्रयास करो। विवेकी बनो। अपने समान साधकों की संगति का आश्रय लो। अपने स्वभाव के लोगों से तथा सात्त्विक वृत्ति वालों से यदा-कदा मिलते रहो। इससे भी आपका विवेक जागृत होगा और आपको वैराग्य-वृत्ति प्राप्त होगी।
परम सत्य की प्रकृति में गवेषणा करो। गीता और उपनिषद् जैसे ग्रन्थों का अध्ययन करो; तब आपको जीवन की समस्त अनन्त समस्याओं का अवबोध हो जायेगा। संसार में सुख अल्पमात्र भी नहीं है। अन्तर्निहित आनन्द की खोज करो।
इस संसार में जनगण सुख की स्पृहा करते हैं। महान् सम्पत्ति के स्वामी होने का कोई माहात्म्य नहीं है। सुन्दर सुगन्धित पुष्पों एवं स्मरणीय दृश्यों तथा सुखद उपवनों से सुशोभित स्विट्जरलैण्ड जैसा अभिगमन स्थान क्या ग्रीष्मावकाश में आनन्दप्रद न होगा ? क्या सुन्दर मनुष्यों का साहचर्य अभीष्ट न होगा। आह्लादपूर्ण न होगा? सुसंगति के अभीष्ट होने पर भी सम्पत्ति और अनुपम स्वास्थ्यप्रद आश्रय तथा आधुनिक मनोज्ञताएँ, पर्याप्त सुख और आमोदक समाज के रहते हुए भी आप देखते हैं कि युवा, मेधावी जनगण जो महान् ऐश्वर्य-साधनों से परिपूर्ण हों, उज्ज्वल भविष्य जिनकी प्रतीक्षा में हो, संसार को प्रिय लगने वाले इन पदार्थों को ठुकरा कर एकान्त, मौन, परित्याग, वैराग्य और आभ्यन्तर ध्यान का जीवन अपनाते हैं। क्यों? इन सर्वपदार्थों को निरर्थक तृण की भाँति पाद-प्रहार करके एकान्तवास और प्रभु में ध्यानमग्न होने के लिए संन्यास क्यों धारण कर लेते हैं? यदि इन पदार्थों में वास्तविक सुख होता, तो ये बुद्धिमान्, ज्ञानी पुरुष ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य न करते। अतः इसकी पृष्ठभूमिका का अवलोकन करने का प्रयास करो। विचार करो, उनकी ओर से ऐसा निर्णय लेने के लिए, ऐसा पग उठाने के लिए और ऐसी जीवन-विधा के वस्तुतः कारण क्या रहे होंगे?
आज भी भारत में सहस्रों स्नातक, युवा डाक्टर और वकील हिमालय की गोद ऋषिकेश में संन्यास-दीक्षा लेने की इच्छा से आते हैं। तदुपरान्त वे ऊपर हिमालय में जा कर गहन ध्यान एवं प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मौन रह कर एकान्तवास करते हैं। क्यों? चिन्तन, मनन, गवेषणा और विवेक द्वारा इन प्रज्ञावान्, विद्वान् तथा विवेकशील पुरुषों ने अपने अन्तःकरण में स्वयं हेतु जो निरूपण किया, आपको चिन्तन द्वारा अपने लिए उसी का निरूपण करना है। गौण तथा तुच्छ पदार्थों का बहिष्कार करके वे अपने जीवन को भगवान् पर केन्द्रित करने में समर्थ थे।
सांसारिक कृत्यों की कलकल तथा प्रचण्ड कोलाहलपूर्ण क्षणों के मध्य भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ प्रशान्त एवं सुख के क्षण भी आते हैं, जब मन उस समय के लिए, चाहे वह कितना स्वल्प भी क्यों न हो, इस संसार के अमेध्य कुत्सित कर्मों से ऊपर उठ कर जीवन की उच्चतर समस्याओं पर विचार करता है तथा जीवन के हेतु एवं लक्ष्य-ब्रह्माण्ड की प्रलेहिका पर चिन्तन करता है। वह खोज प्रारम्भ कर देता है-"मैं कौन हूँ?" सत्यान्वेषी गम्भीर हो कर चिन्तन-निमग्न हो जाता है। वह गवेषणा करता है और सत्य का अवबोध करता है। उसमें विवेक जागृत होता है। अन्ततः वह आत्मा के सर्वोच्च ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु परित्याग तथा वैराग्य के लिए, एकाग्रता और ध्यान तथा कायेन-मनसा शुद्ध होने के लिए तड़प उठता है। किन्तु जिस व्यक्ति का मन लौकिक संक्षोभ एवं भौतिक विचारों से सर्वतः अभिभूत है, वह इन प्रशान्त क्षणों की उपेक्षा करते हुए उनका लाभ नहीं उठाता और अनायास अवश्यमेव आकर्षण और विकर्षण, राग और द्वेष, प्रेम और घृणा के द्वैत भँवर में फँस जाता है और शीघ्र ही सांसारिकता के क्षुब्ध-सागर में आन्दोलित होता है। इस जगत् में विलासपूर्ण जीवन कितना अनिश्चित है! यदि आप इन्द्रिय-सुखों की अनित्य प्रकृति और उनके दोष, दुःख, चिन्ता, क्लेश, कष्ट, उत्सुकता, विकार, अकाल मृत्यु आदि का चिन्तन करें, तो शनैः-शनैः आप अन्तःकरण में वैराग्य जागृत करने में समर्थ होंगे।
आध्यात्मिक आनन्द के विरोधी-विषय-सुख
जैसे प्रकाश और अन्धकार एक ही स्थान पर नहीं रह सकते, वैसे ही ऐन्द्रिक सुखों की विद्यमानता में आध्यात्मिक आनन्द की सत्ता असम्भव है। एक के आगमन पर दूसरे को जाना ही पड़ता है। अतएव सांसारिक विषयों की नितान्त अवज्ञा करो। अन्तःकरण से ही सब इच्छाओं को नष्ट कर दो। मन को इन्द्रिय-विषयों से विमुख करो। तृष्णा का परित्याग करो। मोह त्यागो। आपमें वास्तविक वैराग्य का विकास होगा। आपने स्वयं ही अपना जीवन संकीर्ण और विषम बना दिया है। इच्छाओं, आकांक्षाओं की वृद्धि द्वारा आप संसार-रूपी कीचड़ में फँस गये हैं। जीवन को वैभवपूर्ण एवं असहज बना कर आपने अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को अत्यधिक गुणित कर लिया है। अभिनव आकांक्षाओं को जन्म दे कर आप बन्धन की इस श्रृंखला में प्रतिदिन अधिकाधिक कड़ियाँ जोड़ रहे हैं। सरलता लुप्त हो गयी है। ऐश्वर्यशाली व्यवहार तथा रहन-सहन के ढंग का आलिंगन किया जा रहा है। इसमें आश्चर्य नहीं कि मानव-समाज में सब प्रकार की समस्याएँ हैं। बेकारी, अक्षमता की भावना और अभाव, असन्तोष तथा दुःख सर्वत्र ही दृष्टिगत हैं। व्यापार में अवनमन तथा क्षोभ सर्वत्र है। यह सब मनुष्य की निजी मूढ़ता का ही उद्भव है।
इन असंयत इच्छाओं के कारण मनुष्य सदा असन्तुष्ट रहता है। इन इच्छाओं का कोई अन्त नहीं है। एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से असन्तुष्ट है। कुछ राष्ट्र तो युद्ध की तैयारी में संलग्न हैं। एवंविध, इच्छाओं की वृद्धि तथा वैराग्य के इस महान् सन्देश की उपेक्षा, जीवन को सरल बनाने और अतिरिक्त इच्छाओं का उत्सर्ग कर देने के महान् आदेश की अवेक्षणा न करने के कारण आज मानव-जीवन अनिश्चित हो गया है। मनुष्य अधिक सम्भ्रान्ति, अधिकतर व्यस्तता एवं विमूढ़ता की ओर गतिशील हो रहा है। जीवन सर्वत्र संक्षुब्ध एवं कोलाहलपूर्ण हो रहा है। यह अप्रकट धारा एवं प्रतिद्वन्द्वी धाराओं से परिपूर्ण हो रहा है। क्या इन दुःखों और कठिनाइयों से मुक्ति का साधन नहीं है? एक उत्कृष्ट साधन है- गहन वैराग्य की भावना का विकास। यह मोह-रहित जीवन है। यह सरलता, आत्म-संयम, शुद्धता, निःस्वार्थ-सेवा, स्वार्थ-भाव का त्याग और विश्व-प्रेम का जीवन है।
सम्यक् दृष्टिकोण का विकास करो। सम्यक् चिन्तन, सम्यक् अनुभव, सम्यक् कर्मण्यता आपके स्वभाव का अंग हो। भक्ति और ध्यान का अभ्यास करो। तभी आपको सम्पूर्ण सुख-शान्ति की प्राप्ति हो सकती है। वह अन्यत्र नहीं, किसी और प्रदेश में या निकट भविष्य में नहीं, प्रत्युत यहीं सर्व बाह्य सम्भ्रान्ति (विह्वलता), अशान्ति और जीवन के कोलाहल में सम्भव है। शम और प्रशान्ति तथा वैराग्य और शान्ति से उद्भूत आनन्द के रूप में आप वैराग्य के उत्कृष्ट फल का स्वाद वैराग्य में प्रतिष्ठित हो कर ही ले सकेंगे।
वैराग्य की अपरिहार्यता
इस तथ्य को ले कर हम एक-दो आधुनिक विचारधाराओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे जो वैराग्य के इस विस्तृत विषय से सीधे सम्बद्ध हैं। क्या वैराग्य वस्तुतः अनिवार्य है? इस आधुनिक युग में अगणित जनपद वैराग्य के नाम से ही संकोच करते हैं। इसे अनावश्यक और निरर्थक प्रमाणित करने के लिए वे विभिन्न श्रेष्ठ तर्क प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः वे एक पग और आगे बढ़ते हैं और वैराग्य को हानिकर बताते हैं।
मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैराग्य अध्यात्म का आधार है। हृदय को इच्छाओं से मुक्त किये बिना आप भगवद्-प्राप्ति नहीं कर सकते। आपका अन्तःकरण इच्छाओं से ही परिपूर्ण है, तो आप अमरत्व की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं? परब्रह्म परमात्मा के लिए अनिवार्य ईर्ष्या आप कैसे जागृत कर सकते हैं? इस अभीप्सा के बिना महत् प्राप्ति केवल स्वप्न मात्र है।
आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हेतु वैराग्य अनिवार्य है। सभी धार्मिक और सच्चे गुरु इस तथ्य पर एकमत हैं और बिना किसी भेद-भाव के स्वीकार करते हैं कि भगवद्-साक्षात्कार एवं दिव्य प्रेम की प्राप्ति हेतु मानसिक वैराग्य अत्यन्त ही आवश्यक और प्रचोदक है। इस तथ्य के प्रति सब सुनिश्चित और सुदृढ़ हैं।
आज के युग में किंचिद् सुप्रसिद्ध नेतागण वैराग्य के विरुद्ध आन्दोलन करते सुने गये हैं। किन्तु आप यदि प्रयास करें और इन तथाकथित विद्वान् दार्शनिकों के अन्तर्मन का अवलोकन करें, तो आपको उनमें कूट विषयासक्ति के दर्शन होंगे। निःसन्देह वे बड़े महान् व्यक्ति हो सकते हैं, उच्छ्रित प्रज्ञायुक्त, अद्भुत उपलब्धियाँ प्राप्त महान् प्रशासनिक योग्यता से समन्वित महापुरुष हो सकते हैं; किन्तु वास्तविक महानता कहीं और ही है। महानता इन असाधारण लक्षणों और विशेष गुणों के विकास में निहित नहीं है। हम भूल जाते हैं कि अत्यन्त महान् होते हुए भी वे पुरुष धर्मानुष्ठान के विषय में सर्वथा अशिक्षित हो सकते हैं। मात्र विद्वत्ता धर्म-भाव को उपलक्षित नहीं करती। धर्म किंचिद् गम्भीर वृत्ति है, शीलवृत्ति है। इसका अभिप्राय है अविश्रान्त अभ्यास और अविरत उद्यम, साक्षात्कार के लिए अविच्छिन्न आकांक्षा, वैराग्य पर आधारित सोत्साह अभ्यास एवं वैराग्य से ही प्राणीभूत अनवरत आकांक्षा।
अगणित आधुनिक पुरुष गुरु एवं शिक्षक बने हुए हैं जिनमें वैराग्य-वृत्ति नाम मात्र की है। क्यों? कदाचित् वे स्वयं इच्छाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं। सभी सद्गुरु, वे पूर्वीय हों अथवा पाश्चात्य, आधुनिक युग के हों या अतीत काल के हों-आभ्यन्तर वैराग्य के सम्बन्ध में प्रायः एकमत हैं। इसका बाह्य स्वरूप तो एक पृथक् प्रश्न है, किन्तु सच्चा वैराग्य, सर्व इच्छाओं तथा भौतिक वस्तुओं का सर्वथा परित्याग और तृष्णाओं तथा ऐन्द्रिक उत्तेजनाओं का दाह अत्यन्त आवश्यक है। यही वैराग्य का सार है। सभी प्रबुद्ध गुरु स्वीकार करते हैं कि शाश्वत ब्रह्मज्ञान की अशाश्वत से मोह की उपमा नहीं की जा सकती। दिव्य प्रेम की मात्र प्रतिपक्षी आसक्ति भी दिव्य स्वरूप के साथ पार्श्वपार्श्विक सहवर्तन नहीं कर सकती। इन दोनों का स्थान एक ही तल पर नहीं है, प्रत्युत एक के द्वारा दूसरे का निष्कासन हो जाता है। भगवद्-अनुभूति हेतु हमें लौकिक पदार्थों के प्रति अनन्यमनस्क हो कर इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। भगवान् के अतिरिक्त किसी वस्तु के लिए हमारे अन्तःकरण में यदि अल्पमात्र भी कामना है, तो उसकी अनुभूति असम्भव है। इसी कारण से ईसा अपने आदेश में उनके प्रति अत्यन्त निश्चल थे जिन्हें वे अपने प्रियतम दृढ़ शिष्य बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा-"सर्वस्व त्याग कर मेरा अनुसरण करो। अन्य पदार्थों की ओर उन्मुख न होओ और क्षण-भर के लिए भी मन में उसका ध्यान न लाओ। विरक्त हो जाओ। और मेरा अनुगमन करो।" इनका अभिप्राय है कि हमें अपने हृदय में पूर्ण त्याग उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। केवल तभी प्रभु के लिए सच्ची आकांक्षा, हमारे अन्तःकरण में प्रविष्ट हो कर अनन्यासक्त सत्य, आध्यात्मिक जीवन, सच्चे आध्यात्मिक प्रयास की ओर आगे प्रेरित कर सकती है।
आधुनिक युग के महान् आचार्यों में से एक श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब तक धागे की नोक में एक अल्प तन्तु भी संश्लिष्ट है, तब तक वह धागा सूचिका के छिद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। यद्यपि बाह्यतः केवल एक ही कार्पास-तन्तु संलग्न है, तथापि धागे को पूर्णतया नोकदार किये बिना उसे सूचिका-छिद्र के पार नहीं किया जा सकता। जब तक आपके अस्तित्व की आत्यन्तिक एकाग्रता आपके जीवन के लक्ष्य भगवद्-प्राप्ति की ओर आसक्त नहीं हो जाती, तब तक आत्म-साक्षात्कार में सफलता असम्भव है। अतः अस्पष्ट, सन्दिग्ध प्रकार की नीतियों के प्रति हमें जागरूक रहना है। ऐसे मिथ्या दर्शनालापों से सम्भ्रान्ति के अतिरिक्त अन्य संकट भी उत्पन्न हो सकते हैं।
आधुनिक युग के मिथ्या सिद्धपुरुष
आधुनिक युग भौतिकवादी युग है। आज के युग का एक प्रबल लक्षण अनात्मवाद मूल्यांकन है। अनात्मवाद के भी विविध रूप हैं। एक रूप के अनुसार तो यह जगत् ही सर्वस्व है और केवल यह जगत् ही प्राप्य है। द्वितीय स्वरूप है- सूक्ष्म अनात्मवाद! इसके अनुसार ईश्वर की सत्ता ही पर्याप्त नहीं; इसके साथ ब्रह्माण्ड भी है और आप ब्रह्माण्ड की पूर्णतया उपेक्षा नहीं कर सकते। इस सिद्धान्त के प्रवक्ताओं के अनुसार केवल ईश्वरीय ज्ञान अपूर्णता है। उनके अनुसार वस्तुतः ईश्वर और जगत, दोनों का ज्ञान अनिवार्य है।
ब्रह्माण्ड को जानने का अर्थ क्या है? जिन्होंने इस जगत् को जान लिया है, वे अपने ज्ञान द्वारा सम्भ्रान्त हो गये हैं। आप जगत् को यदि इसके यथार्थ रूप में अवधारण करें कि यह सर्वथा क्षणभंगुर है, अशाश्वत, गमनशील, नश्वर, विपर्यासशील एवं तृणप्राय अर्थात् सारहीन है, तो आप इसमें सुख की खोज नहीं करेंगे। किन्तु ये दार्शनिक कहते हैं कि ज्ञान एकपक्षीय नहीं होना चाहिए और उनके अनुसार, केवल ईश्वरीय ज्ञान एक-पक्षीय है, असन्तुलित है; क्योंकि यह लौकिक ज्ञान से युक्त नहीं है। कदाचित् वे इस तथ्य की अवधारणा नहीं करते कि ईश्वर का ज्ञान हो जाने पर तो अन्य कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता। जगत् तो शाश्वत सत्य परमेश्वर का प्रतिबिम्ब-रूप है और सत्य का बोध हो जाने पर (जो असीम, सर्वव्यापक, अद्वितीय है) सर्व ज्ञान हो जाता है। परन्तु जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य और आत्म-साक्षात्कार के विषय में इन पुरुषों का मत कुछ कुटिल है। उनके अनुसार आपको ईश्वर और संसार दोनों का ज्ञान प्राप्त होने पर ही आपका ज्ञान पूर्ण होगा।
ज्ञान के प्रति कैसी विपरीत विचारधारा प्रचलित हो रही है इन महानुभावों की! इनके कथन का अभिप्राय है आप अमृत और विष दोनों ग्रहण करो। 'दोनों का अनुभव करो' -क्या वे यही कहना चाहते हैं? ईश्वर की अनुभूति होने पर जगत् का अनुभव लुप्त हो जाता है अर्थात् विषयानुभूति की आवश्यकता नहीं रह जाती। जाग्रतावस्था में आप स्वप्नावस्था का अनुभव नहीं कर सकते। वे मिथ्या सिद्धान्त तो स्वप्न को कण्ठ लगाने के समान हैं और इस सिद्धान्त के प्रतिपालक अपने पक्ष को सत्य प्रमाणित करने के लिए अनेक तर्क-वितर्क प्रस्तुत करते हैं। यदि तर्क और अन्य महान् आचार्यों की शिक्षा उनके पक्ष में न हो, तो वे आचार्यों के प्रति पक्षपाती, अज्ञानी, वैधिक (स्वमतावलम्बी) अपवाद कहने में विलम्ब नहीं करते। इन झूठे आचार्यों के हाथों मायावाद के निरूपक महान् आचार्य शंकर भी विवेचना से नहीं बच सके। उनके अनुसार मायावाद के अवधारक शंकर सच्चे नहीं हैं। कम-से-कम मुझे तो इस बात में कदाचित् सन्देह नहीं कि ये पुरुष भगवान् को संसार के साथ जोड़ने में सदा इतने इच्छुक क्यों रहे हैं? कदाचित् उनके अन्तर्मन में संसार के लिए गुप्त अथवा अज्ञानवश इच्छा निहित है। अतः उनके चेतन मन में भी संसार एक गुप्त प्रमाण, एक विशेष मूल्य तथा अर्थ-विशेष से युक्त होता है। अतएव, अभी भी वे इस जगत् में प्रवृत्त रहना चाहते हैं। मन एवं हृदय से इसका सर्वथा उत्सर्ग करने का विचार उन्हें हृदयंगम नहीं होता। इसीलिए उनका वैराग्य अधूरा है, अपूर्ण है और वैराग्य अधूरा नहीं रह सकता। दो प्रपातों के मध्य एक गर्त को दो छलाँगों में आप नहीं लाँघ सकते। केवल एक ही छलाँग में उसे लाँधा जा सकता है, अन्यथा उसे लाँघना असम्भव होगा। इस प्रपात को लाँघने की इच्छा से आप सापेक्षित सत्ता एवं सम्पूर्ण, अनन्त, असीम सत्ता का, लौकिक सत्ता का विभाजन करती हुई किसी प्रकार की आधी छलाँग नहीं लगा सकते।
इन सिद्ध पुरुषों के मस्तिष्क ईश्वर के लिए पूर्णतः उद्यत नहीं हैं। यह स्पष्ट है। एवंविध यह माया का सिद्धान्त और वैराग्य की अनिवार्यता का खण्डन करने का अवगुण्ठित प्रयास तथा यह प्रमाणित करने का यत्न मात्र है कि जगत् भी महत्त्वपूर्ण है, इसकी पूर्णरूपेण उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस द्वैत-विचार से मैं सर्वथा असहमत हूँ। संसार की उपेक्षा करनी ही होगी। इसका अर्थ हिमालय की गुफाओं की ओर भागना भी नहीं है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप सभी सांसारिक पदार्थों का परित्याग कर दें, अपना कुर्ता उतार कर फेंक दें, सामान्य आहार-भक्षण त्याग दें, पत्र-भक्षण प्रारम्भ कर दें अथवा वायु पर ही निर्भर रहना प्रारम्भ कर दें। वैराग्य का अर्थ किसी भी ऐसी विलक्षणता एवं कर्म की अति नहीं है।
आन्तरिक वैराग्य-सच्चा वैराग्य
संसार को त्याग कर भी आप कहाँ जा सकते हैं? आप यदि हिमालय की गुफाओं में जाते हैं, तो भी आप संसार में ही हैं। आवश्यकता संसार के बाह्य रूप से त्याग की नहीं और न ही बाह्य कामनाओं के उत्सर्ग की है। वैराग्य का अर्थ केवल गृह-त्याग, सागर-तट वाटिका, भूभाग विशेष अथवा आहार के रूप का त्याग नहीं है। वैराग्य का अर्थ है-सांसारिकता का सर्वथा परित्याग ! सच्चे वैराग्य का यही रहस्य है।
आप संसार के सर्व पदार्थों का त्याग कर सकते हैं, सर्व सम्पत्ति, समृद्धि, सर्वस्व त्याग कर सकते हैं; किन्तु सम्भव है कि आपका चित्त अभी भी उनमें आसक्त है। आपके अन्तःकरण में इन सब वस्तुओं के लिए आन्तरिक इच्छा हो सकती है। ऐसा वैराग्य सुखद नहीं होता। आन्तरिक वैराग्य के बिना केवल बाह्य वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं है। और यदि आप सम्पूर्ण रूप से आभ्यन्तर वैराग्य में अवस्थित हैं, तो बाह्य वैराग्य निरर्थक है। आप बाह्यतः विरक्त हैं अथवा नहीं, इसका अधिक महत्त्व नहीं है। महानता इस बात में है कि आप संसार में रहते हुए संसार के नहीं हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि विषयों के मध्य रहते हुए भी विषयों की कामना आपके व्यक्तित्व में प्रवेश नहीं करती। ऐसी आकांक्षा का मूल कारण क्या है? यह वैराग्य के विपरीतार्थ में आती है। इच्छा का मूल कारण है, आपके निजी व्यक्तित्व का भाव - 'मैं'। इसी अहं की ही इच्छा, आकांक्षा और तृष्णा का अनुभव होता है। अतएव वैराग्य सब पदार्थ और कर्मों के त्याग में भी निहित नहीं है। यह केवल सामान्येतर आहार ग्रहण करना ही नहीं, यह सम्पन्नता, वस्त्र और जूते का उत्सर्ग नहीं। यह वैराग्य का सार नहीं है। सिर मुंडवा कर संन्यासियों के सदृश वस्त्र धारण करना वैराग्य नहीं है। वास्तविक वैराग्य तो आकांक्षा और तृष्णा, शालीन-प्रकृति, भोग-विलास का परित्याग है जिनका मूल कारण है अहं-भाव- 'मैं' और 'मेरा'। अतः सच्चे वैराग्य का रहस्य अहं-भाव और 'मेरापन' से पूर्णरूपेण मुक्त होने में निहित है। हृदय में 'मैं' की चेतना न हो, 'मैं' का भाव न हो और 'मेरापन' का विचार न हो। मोह और अहंकार का त्याग सच्चे वैराग्य का रहस्य है।
सच्चा वैराग्य सब तृष्णाओं और अन्तःकरण में अवस्थित सूक्ष्म मानसिक संस्कारों तथा पूर्व सुख-भोग के चित्त के संस्कारों का निराकरण है। साधना द्वारा सर्व संस्कारों से मुक्ति प्राप्त करना वास्तविक वैराग्य है। संसार की विकारी वस्तुओं के मोह का त्याग यथार्थतः संन्यास है। सच्चा वैराग्य है-कर्ता, भोक्ता, द्रष्टा, श्रोता एवं गन्धग्राही के भाव (अहंकार) से उपरति, जैसे-"मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं नेत्रों से देखता हूँ; मैं नासिका से गन्ध ग्रहण करता हूँ, मैं कर्णेन्द्रिय से श्रवण करता हूँ आदि।" शरीर एवं इन्द्रियों के साथ इस सरूपता का नाश करना है। यह बन्धन है।
शरीर, मन तथा आकांक्षाओं के साथ एकरूपता को दूर करना है और पूर्णतया शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार से ऊपर उठ कर आपको अपने अस्तित्व को सर्वदा के लिए अपनी ही प्रकृति, अपनी ही सत्य प्रकृति के चैतन्य में केन्द्रित करना है। इन सबसे परे आप सम्पूर्ण हैं, अविकारी हैं, अपरिवर्तनशील साक्षी चैतन्य हैं, जन्म-मृत्यु से रहित, दुःख-रहित, इच्छाओं-आकांक्षाओं से रहित परब्रह्म-स्वरूप हैं (क्योंकि वह सदा पूर्ण और सन्तुष्ट है)।
एक गहन अक्षय तुष्टि आपके वास्तविक स्वरूप को चित्रित करती है। कुछ अभाव नहीं है; क्योंकि यह सर्वतः पूर्ण एवं सम्पन्न है। पूर्णता की जागृति में अवस्थित रहना सच्चे वैराग्य का महानतम रहस्य है। व्यक्तित्व में शरीर-मन की वर्तमान मिथ्या सरूपता का क्रूरता से बहिष्कार करो। अन्तरात्मा में अवस्थित रहो। यही वास्तविक संन्यास है। ज्योतिर्मय आत्मिक चैतन्य, ज्योतिर्मयी आध्यात्मिक प्रकृति स्वज्योतिर्मय दिव्य सत्त्व में समाधिस्थ होना ही सच्चे वैराग्य का रहस्य है। मोह के सब बन्धनों से मुक्ति ही सच्चे वैराग्य की अवस्था है।
५. आत्म-बोध करो
क्षिति-मण्डल की सतह पर स्पन्दनशील और गतिशील जीवन पर यदि आज हम क्षण-भर के लिए दृष्टिपात करें, तो तत्काल ही ज्ञान होता है कि विगत किंचित् शताब्दियों में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है।
मानव ने उन्नति की है, नव स्रोतों का अनुसन्धान किया है, प्रकृति के विषय में पूर्वाभिज्ञान से कहीं अधिक अन्वेषण किये हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि एवं वैज्ञानिक युक्तियों द्वारा उसने ऐसे साधनों का निर्माण किया है जिनके द्वारा अदृश्य पदार्थ भी मानव-दृष्टि के समक्ष अनावृत हो गये हैं। ऐसे शक्तिशाली यन्त्र तैयार किये गये हैं कि प्रायः अदृश्य एवं लौकिक तत्त्व समानरूपेण वैज्ञानिक की मर्मभेदी, सूक्ष्म दृष्टि के समक्ष अभिव्यक्त हो गये हैं। इतनी महान् उपलब्धियाँ इस भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं, पदार्थ-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, विद्युत्-शक्ति आदि में और बाह्य शक्तियों पर मनुष्य ने इतना प्रभुत्व जमा लिया है कि आज जीवन भोग के असंख्य सुख-साधनों से परिपूर्ण है। ऐसी प्रगति, ऐसा शोधन, ऐसी अद्भुत उन्नति हुई है कि शत वर्ष पूर्व भी इस आधुनिक जीवन की कल्पना असम्भव, मनःकल्पित, मात्र भावनोत्पादित रही होगी। उस काल में जो सृष्टि एक स्वप्न मात्र रही होगी, अब साकार हो गयी है।
पुनरपि, दूसरे दृष्टिकोण से विचार करते हुए अब मानव मात्र का ही निरूपण करें। भूमण्डल के विभिन्न भागों में विशाल जनसमूह को हम देखते हैं जो समृद्ध भौतिक वैभव से युक्त हैं; परन्तु उनकी आन्तरिक शान्ति और सन्तोष में अनुरूप वृद्धि नहीं हुई जो बाह्य विज्ञान में उन्नति के परिणाम स्वरूप अपेक्षित थी। मनुष्य यदि समृद्धि और उन्नति की आकांक्षा करता है, तो यह (आकांक्षा) उसे जीवन तथा कर्मण्यता के सब स्तरों, सब दशाओं में करनी चाहिए।
निस्सन्देह, क्षमता बढ़ गयी है और रचना का विस्तरण कर दिया गया है। किन्तु मानव-जीवन में इस संवर्धित सुख की अभिव्यक्ति क्यों नहीं है? वर्गों में आश्चर्यजनक असन्तुलन का राज्य है; किंचिद् वर्ग तो सुख-समृद्धि में क्रीड़ा कर रहे हैं और अन्य वर्ग निकृष्ट निर्धनता में जीवन बिता रहे हैं। एक क्षेत्र में तो प्रचुर सम्पत्ति और समृद्धि का साम्राज्य है, दूसरे क्षेत्र में दरिद्रता और अकाल है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी समृद्धि के साथ दुःख, सुख तथा असन्तोष एक ही समय में दृष्टिगत होते हैं। मनुष्य के वैभव की सामग्री बढ़ गयी है; किन्तु सुखी जीवन के शाश्वत आनन्द में स्पष्ट रूप में कोई वृद्धि नहीं हुई। यदि लोक-परिगणना की जाती, तो सत्यतः कोई भी यह न कहता-"हाँ, मेरे विचार में इस भौतिक प्रगति से हमें शाश्वत आनन्द और केवल सुख की अवस्था प्राप्त हुई है।"
मानव मात्र के दैहिक हित में भी वास्तविक उन्नति अनिश्चित है। चिकित्सालयों की गणना नहीं का जा सकती; चिकित्सक, औषधियाँ, रसायनशाला, औषध-निर्माण एवं शल्य-चिकित्सा के विविध उपाय दशगुणित हो गये हैं; किन्तु रोग द्रुत गति से बढ़े है। विज्ञान में अधिकाधिक प्रगति के साथ नये प्रकार के रोगों और दुःखानुभवों का अतिरेक हो रहा है जो धरती पर मनुष्य को व्यथित करते हैं। क्या इसका भी कोई कारण हो सकता है?
मानव-विश्लेषण की भौतिक उपेक्षा
इसका एक सहज कारण है। अन्ततः मनुष्य इस ब्रह्माण्ड का सबसे महत्त्वपूर्ण प्राणी है। मानवीय कार्यों को दिशा देने की चाबी उसके हाथ में है। आँधी, तूफान, भूकम्प, अनावृष्टि, चक्रवात, महावात आदि आधिदैविक घटनाओं पर मनुष्य का नियन्त्रण नहीं है; परन्तु जहाँ तक मनुष्य के जीवन का प्रश्न है-परिवार, समाज, नागरिक केन्द्र, राजधानी, राष्ट्र अथवा विश्व में सर्वत्र विविध एवं सदा विस्तृत रूपों से सम्बद्ध इस जीवन का नियन्त्रण मनुष्य के हाथों में है। मनुष्य इन कार्यों का निर्देशक है। वह कह सकता है-“जी हाँ, इसी दिशा में चलते रहें" अथवा "नहीं, अब इस दिशा को छोड़ कर उस दिशा में चलें।" जीवन के इस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग 'मनुष्य' का सर्वस्व यथोचित नहीं है। बाह्य प्रकृति के सब क्षेत्रों में प्रगति की जा रही है, किन्तु मनुष्य की अपनी प्रकृति की उपेक्षा हो रही है।
"मानवता के लिए सर्वोच्च अध्ययन मानव है।" मनुष्य को आत्म-बोध करना है। उसे अपनी प्रकृति को समझना है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया में जीवन को प्रशासित करने वाले नियमों का उन्मीलन होता है और मनुष्य के आचार-व्यवहार को निश्चित करने वाले तत्त्वों की अभिव्यक्ति होती है। आन्तरिक शक्तियों के ज्ञान से मनुष्य इन शक्तियों को प्रशासित करने वाले नियमों का प्रतिपालन करना सीखता है और इस प्रकार अपने आचार का समुचित रूप से पालन करता है। यदि यह आवश्यक ज्ञान आकांक्षा और गम्भीर अध्ययन का विषय नहीं बनाया जाता, यदि निज आत्मा का भौतिक ज्ञान उपेक्षित किया जाता है, तब सम्पूर्ण बाह्य पदार्थों का ज्ञान भी चाहे वह कितना ही विशाल या प्रभावशाली क्यों न हो, कदाचित् मनुष्य के संसार में सच्ची प्रगति नहीं ला सकता।
वर्तमान युग में आत्मज्ञान का पूर्णतयां विलोप हो चुका है। मानवीय ज्ञान की इस अक्षमता का स्वाभाविक परिणाम यह है कि मनुष्य अपनी कुल-मर्यादा का अतिक्रमण करने लगा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी, अहंकारी और लोभी बना देती है। सत्ता हथियाने की क्रिया इतनी सामान्य हो चुकी है कि यह भूतल के प्रत्येक भाग में दृष्टिगत होती है। प्रत्येक संकुचित धर्म-समाज अपने ही स्वार्थों की रक्षा कर रहा है। फलतः स्वयं को शेष मानवता का विरोधी बना रहा है। इतना ही नहीं, प्रत्येक समाज अपनी संचित शक्ति को किंचिद् समरूप समाजों के अतिरिक्त अन्य सभी का विनाश करने की भयानक उत्तेजना से क्लिष्ट है।
बीसवीं शताब्दी के प्रथमार्ध के इस मोड़ पर कार्य-कलापों की अनियत अवस्था का यह एक चित्रण है। ऐसा आभास होता है कि वास्तविक प्रगति की अवगति हो गयी है, मनुष्य के स्वभाव में परिशुद्धि के अभाववश वास्तविक प्रगति बाधित हुई है। बाह्य प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में उन्नत होने के साथ-साथ यदि मनुष्य ने आत्मज्ञान भी प्राप्त किया होता, सदाचार को परिशुद्ध करने के साथ उसने प्रेम, दया, परोपकार की क्षमता को बढ़ा कर अपने अस्तित्व की प्रतिष्ठा भी उन्नत की होती और ऐसी प्रगति बाह्य शक्तियों पर प्रभुत्व में प्रगति के समान ही होती, तो आज संसार के सभी समाजों की स्थिति सन्तुलित और कल्याणमयी होती। समृद्धि अधिक होती। बन्धुत्व और मैत्री-भाव और अधिक होता। परस्पर मेल होता।
मानव-समाज द्वारा सृजित बाह्य विकास में असन्तुलन और मूल कुलमर्यादातिक्रमण आज मानवता की दुःखग्रस्त, भयाक्रान्त, अनिश्चित और असुरक्षित अवस्था का मूल कारण है। प्रश्न उठता है-विगत शताब्दियों में इतना अधिक ज्ञान और शक्ति की उपलब्धि करने पर भी, एतत्कालपर्यन्त प्राप्त ज्ञान और शक्ति जो मनुष्य की पहुँच से भी परे थे, सब मानव-हृदयों में यह गहन भाव क्यों समा गया है कि यह समय कदाचित् ही रहने योग्य है। मनुष्य वर्तमान का विचार नहीं करना चाहते। या तो वे भविष्य की काल्पनिक सृष्टि के संकल्प में खोये रहते हैं जिसमें कदाचित् ही मनुष्य ने अपनी सब वर्तमान समस्याओं को सुलझाया होगा, अथवा वे भूतकाल का उत्सुकतापूर्वक चिन्तन करते रहते हैं- "जब दशा श्रेष्ठतर थी।" वर्तमान तो व्याकुलता से आपूर्ण दृष्टिगत होता है। मानव की एक मौलिक भूल के कारण ही यह संस्थिति बनी है। उसके मन की समस्त शक्ति, चिच्छक्ति और इन्द्रिय-ज्ञान को पूर्णत बहिवर्तिन् कर दिया गया है। सर्वप्रथम, उसने समुचित प्रस्थान केन्द्र से ही प्रयास नहीं किया है।
आत्म-बोध के बिना मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं बिता सकता। यह तो उस मनुष्य के समान है जो दीर्घ एवं कठिन यात्रा पर, कदाचित् सहस्रों मील पर्यन्त कार चलाने की कला से अवगत है; किन्तु उस गाड़ी के यन्त्रज्ञान से अनभिज्ञ है जिसने उसे पूर्व पथ पर लाँघ कर लक्ष्य तक पहुँचाना है। प्रत्येक क्षण वह सन्दिग्धावस्था में रहता है; क्योंकि यन्त्र के अनियन्त्रित होने पर वह उसका निरूपण अथवा अनिवार्य क्षतिपूर्ति नहीं कर सकेगा। वही अवस्था आज के उन लोगों की है जो यह तो जानते हैं कि अब दशा बिगड़ गयी है; किन्तु वस्तुतः सुधार के उपायों से अनभिज्ञ हैं। सभी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जन भी लोगों को यह प्रतीति नहीं करा सकते कि इस कार्य में पूर्वस्थिति लाने के लिए उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा कर दी है।
'मैं कौन हूँ' -एक महान् खोज
स्वकीय ज्ञान ही अपेक्षित ज्ञान है। इस ज्ञान की शिक्षा शैशवकाल से ही प्रारम्भ होनी है। शैशवकाल में ही सम्यक् चिन्तन का शिक्षण दिये जाने पर ही व्यक्ति के जीवन में सच्ची उन्नति उद्भूत हो सकती है। सर्वप्रथम हमें यह ज्ञान करना है-हम कौन हैं, हमारे व्यक्तित्व में वे कौन-से तत्त्व हैं जो इसके सौन्दर्य को बढ़ायेंगे और वे तत्त्व कौन-से हैं जो इसका हनन करेंगे। कितने व्यक्ति आत्म-चिन्तन के लिए समय लगाते हैं? जीवन-भर हम अपने संकेत-पालन, सप्ताह भर की योजनाओं, भोग-विलासों एवं प्रियजनों का चिन्तन करते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं-किस प्रकार की नयी पोशाक हम लेंगे, कार का कौन-सा मॉडल खरीदेंगे, भवन में किस प्रकार का रंग करायेंगे। प्रत्येक क्षण बाह्य पदार्थों के ध्यान में ही निरत रहते हैं-प्रतिदिन एकान्त और मौन में कौन आधा घण्टा व्यतीत करता है? कौन पूछता है- "मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? यह कैसा संसार है जिसमें मैं रह रहा हूँ जहाँ कुछ समय पूर्व मैं नहीं था और अब से कुछ समय पश्चात् मैं नहीं रहूँगा? मेरा संसार के साथ क्या सम्बन्ध है? उन पुरुषर्षो से क्या सम्बन्ध है जो मेरे चारों ओर रहते हैं और जिनसे मेरा क्षणिक सम्बन्ध है? इन क्षणिक, नित्य परिवर्तनशील बन्धनों में मेरा क्या कर्तव्य है? इन प्रश्नों का चिन्तन करने के लिए आप समय नहीं लगाते। जब तक आप इनका उत्तर नहीं प्राप्त करते और यह मौलिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते कि आप वस्तुतः क्या हैं, कहाँ से आये हैं और आपका अन्तिम लक्ष्य क्या है, तब तक भविष्य का प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व आपसे कोसों दूर रहेगा। इस संसार से विदा होते समय आप आगमन के समय की अपेक्षा अधिक सुखी न होंगे। इस धरती को आप अपनी विद्यमानता से अधिक उज्वल और प्रफुल्लित करके इसे उन्नत तथा उत्कृष्ट स्थान बना कर नहीं जायेंगे।
आप शरीर नहीं हैं
ये प्रश्न हिन्दू-दर्शन में सदा प्रधान रहे हैं। पुरातन ऋषियों एवं आधुनिक आचार्यों-दोनों ने मनुष्य के भीतर एक जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया है जिससे महत् आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु भौतिक जीवन का सदुपयोग किया जा सके। अज्ञानी, मूढ़, निर्बुद्धि एवं मूर्ख शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। मनुष्य अपने प्रति यही सोचता है-"मैं पाँच फुट नौ इंच लम्बा हूँ, मेरा भार इतना है, आयु इतने वर्ष है आदि।" स्वयं को इस अस्थियों के नाशवान् पिंजर, हाड़-मांस, नाड़ी और चमड़ी की इस स्थूल देह से समरूप मान लेने के अतिरिक्त इससे बड़ी मूर्खता, अज्ञान, अन्धकार अथवा मन्दमति और क्या हो सकती है? पुनरपि, यदि नश्वर अन्न पर पूर्णतया निर्भर न हों, तो यह भौतिक विधान और क्या है? अन्न प्रवेश होने पर शरीर का विकास होता है; किन्तु इसका संहरण करने पर शरीर शान्त हो जाता है। क्या आप यह हैं- यह पूर्णतया विषय स्वरूप जो पूर्ण रूप से उन पदार्थों पर निर्भर है जो स्वयं नाशवान् हैं? किन्तु अधिकांश व्यक्ति ऐसा ही करते हैं।
आप यह शरीर नहीं हैं। यह शरीर तो किंचिद् समय पूर्व ही अस्तित्व में आया। इसका प्रारब्ध तो अचिरेण ही विश्लिष्ट और विनष्ट होना है। आप ? आप यह शरीर नहीं हो सकते। आप कदापि ऐसा अनुभव नहीं कर सकते कि आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। अस्तित्व के न होने का विचार भी आपके लिए अविचारणीय है। आपके स्वभावानुसार ही ऐसा विचार आत्यन्तिकरूपेण अबोधगम्य तथा असम्भव है। आपकी चेतना ऐसा विचारने की आपको कभी भी आज्ञा न देगी; क्योंकि इस प्रकार की धारणा, कि आपका अस्तित्व नहीं है, बना लेने पर भी आप स्वयं को इस कथन का निर्माता समझते हैं। आप स्वयं को मात्र इस विचार से भी परे अनुभव करते हैं।
यह मूर्खतावश है। अज्ञान अन्धकार, मात्र अविचारणा है कि मनुष्य शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। शरीर आपका दृग्विषय है। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं अथवा इसके प्रति बात कर सकते हैं जिस प्रकार आप एक मेज अथवा कुर्सी की ओर निर्देश करेंगे। अतः यह कर्ता, द्रष्टा अथवा लक्षक नहीं हो सकता। पुनरपि आप कह सकते हैं-"मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा शीर्ष", और विकलांग हो जाने पर आपको यह अनुभव नहीं होता कि आपका विलोप हो गया है। व्यक्तित्व का कोई पक्ष अंग च्युत होने पर कम नहीं होगा। पुनरपि आप ऐसा ही अनुभव करेंगे कि आप पूर्ण स्वस्थ, अक्षत और अविकल हैं। आप इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि आप इस शरीर के दर्शक हैं जो आपका मात्र दृग्विषय है।
आप मन नहीं हैं
चेतना इन्द्रियों के वशीभूत नहीं हो सकती। क्या आप दर्शन, घ्राण, स्वाद, स्पर्श, श्रवण आदि कर्मेन्द्रियाँ हो सकते हैं जिनका केन्द्र मस्तिष्क में है और जो इन्हें कार्यार्थ प्रेरित करता है? आप यदि श्रवण नहीं कर सकते, तो श्रवण-शक्ति खो देने से आप अपने व्यक्तित्व को नहीं खो देते, एवंविध दर्शन एवं प्राण-शक्ति की हानि से आपके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप गहन सुषुप्तावस्था को प्राप्त होते हैं जहाँ सभी दश कर्मेन्द्रियाँ अकिंचित्कारी एवं मृतप्राय होती हैं, तब भी 'आप' वहाँ विद्यमान होते हैं। आप अपना सतत अस्तित्व रखने में समर्थ होते हैं। जागने पर आप कहते हैं- "मैं ही सो गया था और अब स्वयं को जगाने वाला मैं ही हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं सुखपूर्वक सोया।"
यह 'मैं' क्या है जिसका अस्तित्व गहन निद्रा, स्वप्न रहित सुषप्ति में भी बना रहता है, जब कि शरीर का चैतन्य और बाह्य संसार नहीं रहते और मन के कार्य उपराम हो जाते हैं? गहन निद्रा में, जब शरीर पूर्णतया निष्कर्मण्य होता है, जब इन्द्रियाँ और मन कर्मशील नहीं होते और जब बुद्धि भी और अधिक कर्मशील नहीं रहती, तब भी आपका अस्तित्व रहता है। जागने के तत्काल पश्चात् ही आप अपने व्यक्तित्व-चेतन की डोर सँभाल लेते हैं मानो यह कभी परोक्ष हुई ही नहीं और आप कहते हैं- "मैं सो गया था और मुझे अतीव आनन्द मिला। अब मैं गतश्रम जागृत हुआ हूँ।" मन, बुद्धि और कर्मेन्द्रियों से परे स्वतन्त्र यह कौन-सा रहस्यपूर्ण तत्त्व है जो आपको अपने अस्तित्व की शाश्वत चेतना का आभास कराता है? स्मृति-नाशक औषधि के प्रभाव से पूर्णरूपेण स्मृति-भ्रंश होने से पूर्व अस्तित्व की सभी वस्तुएँ प्रक्षालित हो कर चेतना से विलुप्त हो जाती हैं (मानो लेख-पट्टिका पर लिखित लेख मिटा दिया गया हो), तब मनुष्य कहता है- "मैं नहीं जानता" अथवा "मुझे स्मरण नहीं। "यह 'मैं' की जागृति क्या है जो सर्व महत्त्वपूर्ण तत्त्व स्मृति-सहित व्यक्तित्व के सभी पक्षों से स्वतन्त्र है?
सार्वभौमिक तत्त्व 'मैं' और 'मैं हूँ'
अध्यात्म की गहराई में उतरने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह 'मैं', आपका अपना जीवात्मा समस्त मानवता एवं सर्व भौतिक प्राणियों से इतना निकट रूप से सम्बद्ध है कि सार्वभौमिक रूप से विविध राष्ट्रों, जातियों, धर्मों, मतों एवं वर्णों के विस्तृत समूह की कल्पना करें तो नाम, रूप, परिमाण, विचारधारा, वर्ण, जाति, पोशाक, खाने, पीने, सोने का ढंग, संक्षेप में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सर्वथा पृथक् है। आप अचरज करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सर्वथा भिन्न होते हुए भी 'मैं, मैं, मैं' अथवा 'मैं हूँ' की रट लगाये रखता है। वह अफ्रीकी हाटेन्टाट हो या अलास्का का एस्किमो, मलेशियन हो या अरब निवासी, यूरोपियन हो या कैनेडियन, हिन्दू हो या बौद्ध, अनिवार्यरूपेण 'मैं' का प्रयोग करेगा। अतएव 'मैं' और 'मैं हूँ' का यह भाव उन तत्त्वों के समान नहीं है जो लोगों को छिन्न-भिन्न करके विशिष्ट प्रकार से पृथक् कर दे। यह निश्चयरूपेण सामान्य सार्वभौमिक तत्त्व है। यही तत्त्व है जो मानवता को सूक्ष्म एकता में संग्रथित करता है।
मिथ्या ऐक्य-भाव सार्वभौमिकता को नष्ट करता है
हमने प्रत्येक व्यक्ति को 'मैं' और 'मैं हूँ' कहते सुना है, और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया सत्य है और प्रत्येक अन्य भौतिक प्राणियों के साथ एकचित्त है। किन्तु इस द्वितीय शब्द से आगे मनुष्य अपनी अज्ञानता का परिचय देता है। वह (इन शब्दों के साथ) प्रगमन करता है- "मैं एक अमरीकन हूँ", "मैं कनाडावासी हूँ", "मैं हिन्दू हूँ", "मैं प्रजातन्त्रवादी हूँ।" 'मैं' के पश्चात् लिखित उपाधि तत्काल उसकी चेतना को सीमित कर देती है। यह ऐक्य-भाव के चैतन्य को दूषित कर देती है। एवंविध जब आप कहते हैं-"मैं हूँ", आप मानवता के साथ एक होते हैं; किन्तु जब आप कहते है-"मैं अमुक हूँ", आप स्वयं को पृथक् करके स्वयं तथा स्वयं से विपरीत मनुष्य के मध्य एक सीमा स्थापित कर देते हैं। आप तत्काल ही स्वयं को शेष संसार से पृथक् कर लेते हैं और अन्य जनों को स्वशत्रुवत्, विपक्षी और दुष्टतर तथा अपना हितकारी आदि समझने लगते हैं। यहीं बृहत् अज्ञान अवस्थित है। इसी में विचार की नितान्त शुद्धि की आवश्यकता प्रतीत होती है। यहीं पर आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है।
आपकी बुद्धि ही जीवन में यदि आपकी मित्र और सखा हो, तो निम्न प्रज्ञा एवं इच्छा प्रकृति के काम और मोह में अवगुण्ठित तथा बन्धग्रह करने वाले व्यक्तिगत इच्छा-अनिच्छा तथा मोह-माया के आवरण से अनावृत अत्यन्त शुद्धतम रूप में इसका प्रयोग करने पर यही बुद्धि आपको महती सेवा प्रदान कर सकती है। यदि आपकी प्रज्ञा, आपका शुद्ध विवेक एवं ज्ञान-शक्ति निम्न प्रकृति में संश्लिष्ट हैं और इस प्रकार अपनी स्वाधीनता से वियुक्त हैं, तो अहं-भाव का शुद्ध चैतन्य दूषित हो जाता है। प्राणिमात्र के साथ सार्वभौम एकत्व के भाव का विलोप हो जाता है। आपकी बुद्धि आपको अन्य पुरुषों के प्रति स्वार्थ, आसक्ति, घृणा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, क्षुद्रता, निकृष्टता, निर्दयता और हीनवृत्ति के पाश में बाँध कर आपको दुःखों की श्रृंखला में बाँधती है। बुद्धि के कलुषित प्रभाव के कारण ऐसे अशुद्ध भाव जागृत होते हैं और मानव-व्यक्तित्व में पार्थक्य-भाव तथा चैतन्य-संकोच को जन्म देते हैं।
पुनः, 'मैं हूँ' का भाव आपको सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से ऐक्य-भाव की अनुभूति कराता है; परन्तु आपका यह कथन-"मैं मनुष्य हूँ", आपको एक जाति-विशेष में परिसीमित कर देता है और वह है-मनुष्य जाति! आप सोचते हैं-"मैं वह प्राणी नहीं हूँ" और कहते हैं- "उस श्वान पर पदाघात करो", "उस मूषक को मार 7 ^ prime prime , "उस खटमल को कुचल दो", "उस खरगोश को बन्दूक से मार दो।" एवंविध आप स्वयं को अन्य सभी प्राणियों से पृथक् कर लेते हैं और पुनः स्वयं को 'मनुष्य' की संज्ञा देते हुए आप कहते हैं-"मैं श्वेत हूँ", अश्वेत जाति का पूर्ण संसार मानो आपसे भिन्न हो जाता है। आप दीवार खड़ी करते हैं और वहाँ भी वह समाप्त नहीं होती। आप अपनी चेतना को पुनः यह कहते हुए संकुचित करते हैं कि आप एक फ्रांसीसी हैं, अमरीकी हैं, फारसी हैं अथवा न्यूयार्क-वासी हैं, आप संकीर्ण-से-संकीर्ण होते चले जाते हैं यहाँ तक कि आपका हृदय विशाल होने की अपेक्षा संकुचित और सीमित होता चला जाता है। इसका आशय यह है कि आप अपने सत्त्व को संकुचित करने और शुद्ध चैतन्य तथा स्वाभाविक आध्यात्मिक तत्त्व की सार्वभौमिकता का गला घोंटने की प्रक्रिया में अग्रसर हो रहे हैं। यही मृत्यु है। अपनी आत्मा को छोटे-से-छोटे वृत्तों में सीमित करना जीवन के नितान्त मूल में अथवा आदिहेतु में जा कर उसका कण्ठावरोध करने के प्रयास के समान है। जीवन-स्रोत समग्र विश्व में व्याप्त और प्रवाहित हो रहा है; किन्तु इसके स्वाभाविक और सहज प्रवाह को अवरुद्ध करते हुए आप स्वयं को सीमित करके शान्ति की धारावाहिक आन्तरिक आभ्यन्तर अभिव्यक्ति को निग्रहीत कर रहे हैं। त्वचा का वर्ण, सम्प्रदाय, कक्षा, वर्ग अथवा धर्म आदि स्व-अस्तित्व के इन गमनशील स्वरूपों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए आप अपने ही सार्वभौमिक चैतन्य की विशालता एवं चित्तोल्लास को खो रहे हैं। आप स्वयं को आत्मा के सत्य तथा उत्तुंग अनुभव से च्युत करते हैं। फिर आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपनी आत्मा की दुर्बल, अपर्याप्त, मिथ्या छाया का ज्ञान है। आप फिर आँसु बहाते हैं; क्योंकि आप जीवन के नितान्त नियम के ही विरुद्ध चलते हैं।
विस्तरण सुख है। एकत्व सुख है। क्षुद्र स्वजीव से बाहर आना निर्भीक होना है। जितना अधिक आप स्वयं को व्यक्तित्व की संकुचित धारणा में प्रतिबद्ध करते हैं, उतनी ही सुदृढ़ परिसीमा आविर्भूत होती है। तब भय, भेद-भाव, शत्रुता और घृणा आनी स्वाभाविक है। जीव की शाश्वत प्रकृति-शान्ति का लोप हो जाता है। चैतन्य की परिसीमा द्वारा जब प्रेम का इस प्रकार विरोध होगा, तो सुख कहाँ से आ सकता है? यह प्रेम ही है जो मनुष्य के जीवन में प्रकाश और सुख प्रवाहित करता है। प्रेम आपके अस्तित्व की नित्य प्रकृति है।
आप सत्-चित्-आनन्द हैं
अब इतना स्पष्ट हो गया कि आप जब कहते हैं-"मैं हूँ", तो आप अपनी सत्ता को प्रतिपादित करते हैं। यह सत्ता आपकी वास्तविक प्रकृति है और यह शाश्वत है। यह सत्ता अनश्वर है; क्योंकि पंचतत्त्वों से युक्त शरीर की भाँति इसकी रचना नहीं हुई है। आपकी सत्ता के अशाश्वत तत्त्वों, जैसे शरीर आदि से इसका तादात्म्य न होने के कारण यह उन सबसे स्वतन्त्र है। यह अपरिवर्तनशील है। मन सतत परिवर्तनशील है। यह नये विचार धारण एवं पुरातन विचारों का प्रक्षेपण करता रहता है। आपके मस्तिष्क में अनवरत स्पन्दन होता रहता है। सदा परिवर्तन गति और स्पन्दन की अवस्था में रहने वाला यह मन आपके भीतर शाश्वत तत्त्व नहीं हो सकता। शाश्वत तत्त्व सत् है। आप अविनाशी, अनश्वर सत्ता हैं। शाश्वत जीवन आपका सत्य तथा अनिवार्य सत् है। वही आपकी प्रकृति है।
आप चित्-स्वरूप अथवा जागृति भी हैं। आप जड़ अथवा अचेतन नहीं हैं। आपको अपनी सत्ता की प्रतीति है; अतएव आपमें ज्ञान भी है। यह आपकी शाश्वत प्रकृति का एक अंश है। अतः आपकी सत्ता है और आप अपनी सत्ता के प्रति चेतन हैं। आपको अपनी सत्ता का ज्ञान है। आप आत्मज्ञ हैं।
आप सत् हैं, चित् हैं, आनन्द हैं। जब आपको यह ज्ञान होता है कि आप पवित्र सत्-चित्-स्वरूप हैं और साथ ही जब आप यह जान लेते हैं कि आप वह तत्त्व नहीं हैं जो आपको निरन्तर उत्तेजित कर रहा है, तब आप सम्भवतः अपने जीवन के निम्नतर नश्वर पक्षों के दोषों तथा अपूर्णताओं से मुक्त हो जाते हैं। सब प्रकार की पीड़ा, दुःख, भय, शोक और क्लेश शरीर के लिए हैं। कष्ट सहन करना ही देह की नियति है। ईर्ष्या-द्वेष, मोह, शोक, इच्छा, सुख और दुःख का अनुभव करना मन के भाग्य में है। आप जब स्वयं को शरीर और मन-दोनों से स्वतन्त्र और पृथक् समझते हैं, तो अपने निम्न अस्तित्व को चित्रित करने वाले इन दो पक्षों को आप क्या आज्ञा देंगे कि वे आपकी जीवात्मा को अधीन कर लें अथवा स्पर्श भी करें? मन और बुद्धि को लक्षित करने वाले सभी दोषों जैसे पीड़ा, कष्ट, दुःख, मोह, इच्छा, अनिच्छा आदि से आप स्वतन्त्र हो जाते हैं। इस प्रकार नित्य रूप से आप आनन्द से परिपूर्ण हैं। आपकी वास्तविक प्रकृति आनन्द है। आप सत्-चित्-आनन्द (सच्चिदानन्द)-स्वरूप है।
यह 'मैं' आपकी सत्ता के शरीर और मन वाले भाग से पृथक् तथा सर्व मलिनताओं एवं दोषों से मुक्त है। सम्भव है मनुष्य होने के नाते आपको अपनी सत्ता के निम्न स्तरों के दुःख, विपर्यास और परिवर्तन अनुभव करने पड़ें; किन्तु आप आनन्द-स्वरूप हैं और उस आनन्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये अनुभव केवल मन तक ही सीमित हैं और यदि आप आज्ञा दें तो बुद्धि तक पहुँच सकते हैं; किन्तु इससे परे वे नहीं जा सकते। वे आपको स्पर्श नहीं कर सकते। वे आपकी दूरस्थ आत्मा तक नहीं पहुँच सकते; क्योंकि वस्तुतः आप सच्चिदानन्द-स्वरूप हैं, शाश्वत और पूर्ण, शुद्ध एवं अविकारी हैं। इसी स्वरूप में आत्म-बोध करो। निश्चयेन, मनुष्य की वास्तविक प्रकृति यही है।
आप अभी भी भगवत्स्वरूप हैं
यह बोध सर्वोच्च, प्रकाशमय आत्मा की प्रकृति को होता है; किन्तु प्रकृति मेधावी अथवा विवेकी पुरुष की भी यही होती है, यद्यपि वह प्रायः किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है और उसके प्रति कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसे ज्ञान है और दूसरे ही क्षण ऐसा आभास होता है कि उसे ज्ञान नहीं है। विचार करने की प्रक्रिया से भी अनभिज्ञ अशिक्षित, अज्ञानी पुरुष भी इसी प्रकृति से युक्त है। मूर्ख एवं अनात्मज्ञ की भी यही प्रकृति है। आप अन्तःकरण में आध्यात्मिक चैतन्य के उद्भव, उन्मीलन और अभिव्यक्ति की किसी भी अवस्था को प्राप्त करें, अन्तस्तल में मूलतः, सत्यतः, यथार्थतः इस क्षण भी सच्चिदानन्द हैं। उस (सच्चिदानन्द) प्रकृति का अपहरण नहीं हो सकता।
यह ज्ञान आपकी महानतम पूँजी है। यह पूँजियों की पूँजी है। आपने इसी का ही तो उन्मीलन करना है। इसी का साक्षात्कार करने के लिए आप यहाँ आये हैं। आप स्वय को जानने के लिए (आत्म-बोध करने के लिए) यहाँ आये हैं। यह सत्य आपको मुक्त कर देगा। वस्तुतः आप नित्य मुक्त हैं, अभी भी मुक्त हैं; क्योंकि यह सत्य इस तथ्य से असम्बद्ध है कि आपको इसका ज्ञान नहीं है। इस सत्य को कोई चुरा नहीं सकता। यह सदा सत् है। आपका अज्ञान आपके अस्तित्व की पूर्णता को लेशमात्र भी अभिभूत नहीं करता।
स्व-अस्तित्व की सत्यता के विषय पर आपको चिन्तन, मनन करना चाहिए। इस पर ध्यान करना चाहिए। इसका साक्षात्कार करना चाहिए। सर्वोपरि, आपका जीवन इस आभ्यन्तर सत्य की अभिव्यक्ति होना चाहिए। आपके जीवन में आपकी आन्तरिक आनन्दमयी प्रकृति का अनवरत प्रदर्शन होना चाहिए। केवल उस स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं जो आपका अभिन्न अंग नहीं, यद्यपि मनुष्य होने के नाते आपमें ये दोनों पक्ष विद्यमान हैं। आप अपने अस्तित्व के उस मिथ्या अंश से भी पृथक् नहीं हो सकते जिसका आदि है और अन्त भी है, जो कुटिल और नश्वर है।
आपकी वास्तविक एवं अद्वितीय प्रकृति का सार्वभौमिक चैतन्य से तादात्म्य है जिसे लोग परमात्मा जान कर उपासना करते हैं और अन्योन्य नाम-अल्लाह, जेहोवा, ईश्वर, ब्रह्म तथा सर्वशक्तिमान् पिता के नाम से पुकारते हैं। यह तो परमात्मा ही है, आप उसे कोई भी संज्ञा दें। वह परम, असीम, शाश्वत पूर्ण सत्ता है। वह सर्वात्म रूप है। सम्पूर्ण मानवता में लीन वह एक ही चैतन्य है जो मानव मात्र को संग्रथित तथा संयुक्त करके सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को सुख से आपूरित करता है। वह हर्षोल्लास का महान्, अविरत, अक्षय भण्डार है।
आत्मिक प्रकृति में आप वही हैं। सुख, आनन्द और ज्ञान के असीम भण्डार से आप शाश्वतरूपेण सम्बद्ध हैं। इसका साक्षात्कार करने पर आपका जीवन प्रेम के प्रकाश, आनन्द, ज्योति, सुख, शान्ति और सौम्यता के ओज से प्रदीप्त हो उठता है। प्रतिदिन इस तथ्य पर विचारने का नियम बना लो कि आप वस्तुतः कौन हैं? आत्मा को परमात्मा में केन्द्रित करो। सत्-स्वरूप आदिहेतु से तादात्म्य स्थापित करो जो कुश की धार, धूल के कण, मेघ-समूह और जीवन के प्रत्येक भाव तथा अभिव्यक्ति में विद्यमान है। स्वयं को दूसरों से एकरूप मान कर आप उन्हें आघात कैसे पहुँचा सकते हैं? आप स्वयं को मिथ्या और अत्याचारी कैसे बना सकते हैं? आप स्वयं को छद्मी और अनृप्त कैसे बना सकते हैं? निज आत्मा को ही घृणा और क्रोध करने के लिए आप कैसे प्रेरित कर सकते हैं?
प्रभु के संग चलो, प्रभु के संग सम्भाषण करो
व्यष्टि एवं समष्टि रूप से आज मानव को इसी विचार, इसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जब प्राध्यापक ईस्टन को एक बार एक इन्टरव्यू में पूछा गया-"महोदय, विश्व की उन्नति के लिए क्या हल करेंगे?" उसने कहा- "हमें लोगों का सुधार करना चाहिए था।" इसका आशय है, हमें चैतन्य-रूप से अपनी सात्त्विक प्रकृति में अवस्थित रहना चाहिए। यदि कुछ मुट्ठी-भर लोग भी यह दृढ़ धारणा तथा स्वजीवन का महानतम लक्ष्य और आकांक्षा बना लें कि अब और अधिक, मात्र भौतिक प्राणियों की भाँति न रह कर स्वयं में दिव्यानुभूति करनी है, सदा दिव्य सत्त्व प्रभु के साथ तादात्म्य हो कर रहना है, तो सच्चे शब्दों में उन्नति हो सकती है। प्रतिदिन इसी प्रकार से जिओ।
निश्चय करो कि आप स्वयं को यह शरीर अथवा इन्द्रियाँ नहीं समझेंगे। आप स्वयं को इच्छा और भ्रान्ति से युक्त अपूर्व चेतन नहीं मानेंगे। आप सदैव अपने वास्तविक सत्य-स्वरूप का अनुभव करेंगे। यदि आप ऐसी धारणा बना लें, तो आपका सम्पूर्ण जीवन प्रकाशमय हो जायेगा। आपका सदन जगमगा उठेगा। आप जहाँ भी जायेंगे, जनगण देखेंगे कि आप अपने साथ तेज लाते हैं। रुग्ण व्यक्ति स्वस्थ अनुभव करने लगेंगे। आप परम सत्य के ज्योति-प्रसरण हेतु केन्द्र बन जायेंगे।
आप यहाँ देवतुल्य जीवन यापन हेतु अवतरित हुए हैं। देवताओं की भाँति अभिनय करो तथा देवताओं की ही भाँति अनुभव करो; क्योंकि निश्चयेन आप दिव्य स्वरूप (परमात्मा) की सन्तति हैं। सम्पूर्ण रूप, सबसे पवित्र, सर्वचैतन्य और सर्वज्ञ प्रभु के साथ आप सदा एक हैं। यह महान् तथ्य आपके जीवन का प्रमुख सत्य है। यह प्रत्येक मनुष्य के अन्तःकरण की अनुपम पूँजी है। आपको ऐसा अनुभव करना चाहिए कि आप अन्तस्तल से दिव्य सत्त्व का प्रकाश बिखेर रहे हैं। भगवान् की आँखों से देखो। प्रभु की अनुभूति से स्पर्श करो। परमात्मा की प्रकृति से आपका अन्तःकरण झनझना उठे। इसमें समस्त मानवता के लिए प्रेम भरा हो।
आत्मज्ञान, आनन्द के अक्षय स्रोत के साथ योग की अनुभूति है। मौन में (एकान्त में) ज्ञान करो कि आप दिव्य हैं। तत्पश्चात् उसी मौन में रहो। महत्तर साक्षात्कार की आनन्दमयी जागृति में दिन-प्रतिदिन संवर्धन करो। अन्ततोगत्वा ऐसा जीवन आपकी चेतना को सार्वभौम चैतन्य में विस्तृत कर देता है। वैश्विक चैतन्य की प्राप्ति इस सत्य का ज्ञान है। आप परमात्मा के अभिन्न अंग हैं। जीवन के प्रत्येक अन्य कृत्य (कर्म) का सापेक्षिक महत्त्व है। कदाचित् इस पिंजरे में फँस कर हम अन्य कमाँ की पूर्णतया उपेक्षा न करें; किन्तु वे केवल गौण कर्म हैं। इस जीवन के तथाकथित कर्मों को यदि आप बिना आत्मज्ञान के करते हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है; किन्तु आपके अपने विनम्र परिमाण से यदि आपका अन्तःकरण इस सत्य का अनुसरण, प्राप्ति और अनुभूति, आपकी अपनी सत्ता के रूप में कर लेता है, तो आप अन्य कर्मों के अनुष्ठान में स्वतन्त्र हो जाते हैं। आपका जीवन पूर्ण गरिमामय एवं सफल हो जाता है। आपके साथ रहने वाले मनुष्यों के लिए आपके अन्तःकरण से आशीर्वाद प्रस्फुटित होंगे।
जीवन को ही दिव्य बनाना आपके भौतिक अस्तित्व का एकमात्र धर्म है। दिव्यता से आपके जीवन का अवतरण हुआ है। सदेहावस्था में भी दिव्य जीवन व्यतीत करो। शाश्वत दिव्यता आपका सर्वोच्च लक्ष्य है। दिव्य ओज में प्रतिष्ठित होने पर जीवन को उसी ओजस्विता में बहने दो। आपका जीवन उस अनन्त की पूर्ति से सुशोभित हो उठे। आनन्द और सत्य ही आपके मात्र अनुभव हों। इस विश्व में, जहाँ हम वास करते हैं, आप शान्ति, सौम्यता और प्रेम की वृष्टि करें! आत्म-बोध करें, दिव्य बनें, देवतुल्य आनन्द-स्वरूप बनें!
६. आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य
गरिमामय अमर आत्मन्! इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से परे एक शाश्वत सत्य निहित है जो आपके समक्ष विद्यमान है। नाम और रूपों से निर्मित जिस जगत् का आपको ज्ञान है, उससे अतीत विराट् सजीव तत्त्व विद्यमान है। महान् सत्य, सजीव तत्त्व की प्रकृति परम सुखद एवं आनन्दमयी है। यह बन्धन-रहित मोक्ष, असीम शान्ति, अनन्त ज्ञान तथा अनिर्वचनीय आनन्द की अवस्था है। यह वह सुख है जो सुदूर धरातल पर्यन्त अनुपमेय है। और वह आनन्द, स्वतन्त्रता, शान्ति, ज्ञान और सुख आपकी अनवरत शाश्वत अवस्था है। वह आपका परम धाम है। वही आपका परम लक्ष्य है। उस अवस्था की प्राप्ति ही आपके जीवन का उद्देश्य है। उस परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए आपको यह जीवन मिला है। इसी साक्षात्कार द्वारा अन्ततोगत्वा इस भूलोक के दुःख और विपत्तियों को अतिक्रमण करने की शक्ति प्राप्त होती है। एक ही शब्द में, आपके जीवन का लक्ष्य 'भगवद्-साक्षात्कार' है। यही और केवल यही उपलब्धि आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। सब मलिनताओं, पापों और दुःखों के होते हुए भी इस धरती पर मनुष्य-जीवन के उद्धार का यह एकमात्र सच्चा साधन है। सत्य तो यह है कि जीवन उस परमात्मा की प्राप्ति का एक उज्वल साधन मात्र है जिसके द्वारा वास्तविक और निर्मल सुख की अनुभूति की जा सकती है।
सुख की महान् खोज
आइए, जीवन का निरूपण करें! हमारे निरूपण से कौन-सा महत्त्वपूर्ण तत्त्व परिस्फुटित होता है? वह यही है कि मनुष्य कहीं भी रहे कर्मण्यता भी साथ ही सुस्पष्ट है। लोग भाग-दौड़ में लगे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति काम के बोझ से दबा जा रहा है। विश्राम अथवा चिन्तन के लिए क्षण-भर भी नहीं है। यह कैसी कर्मण्यता है? आइए, इसका विश्लेषण करने का प्रयास करें। इसमें से अधिक कर्म सुख, भोग तथा आनन्द के विविध स्तर एवं प्रतिच्छाया रूप अनुभव की उत्तम खोज हेतु होते हैं। साथ ही, मानव स्वयं को दुःख, पीड़ा और क्लेशों से मुक्त करने के लिए अनवरत चेष्टा में संलग्न है। असुखकर, क्लिष्ट, दुःखावह और शोकपूर्ण, सब तत्त्वों के परिहार एवं आनन्दकर, सुखद, हर्षपूर्ण एवं भोग्य पदार्थों की प्राप्ति हेतु मनुष्य यत्नशील है। ऐसा करना तर्कपूर्ण है कि मनुष्य सप्ताह में व्यवसाय के सभी पाँच दिन स्वेच्छा से ही पर्याप्त क्लेश और अविश्राम मोल लेता है और कठिन परिश्रम करने के लिए भी बहुत प्रयास करता है। वह अनेक दुःसाध्य कार्य सम्पन्न करता है। अतः यह कथन कहाँ तक उचित है कि वह दुःखद और उद्देश्यपूर्ण अनुभव का निराकरण करने का प्रयास कर रहा है। किन्तु, किंचिद् गहराई में जा कर उसके सोद्यम संघर्ष के उद्देश्य की खोज करें। अपने इन सब प्रयासों और श्रम द्वारा मनुष्य अपने भविष्य को लक्षित करके भावी जीवन को विश्रामप्रद, सुखद और वैभवशाली बनाना चाहता है। यह सभी प्रयास धनार्जन की ओर लक्षित हैं; क्योंकि धन से कदाचित् अधिकाधिक सुख अपेक्षित हैं।
इन बातों से हमें किंचिद् बोध होना चाहिए कि जीवात्मा की वास्तविक प्रकृति आनन्द है। सदेह सत्ता में आनन्द की यह यथार्थ प्रकृति कुण्ठित हो जाती है। शरीर और इन्द्रियाँ ससीम हैं। हमारे ऊपर उष्ण एवं शीत, बुभुक्षा एवं पिपासा, व्याकुलता एवं रोग रूपी दोष आरोपित हैं। मानसिक ताप भी है जैसे-शोक, वियोग और विषाद, अपने प्रिय जनों का वियोग, अप्रिय जनों का संयोग जिनसे हम व्याकुल रहते हैं, चिन्ता, भ्रम, ईर्ष्या, असफलता आदि। इस सदेहावस्था में यह तत्त्व हमारी सर्वानन्द-स्वरूप सच्ची प्रकृति पर आवरण-सा डाल देते हैं, यद्यपि हम अवचेतन मन से सर्वदा अपनी सच्ची, गुप्त उच्च प्रकृति का प्रतिबोध करके प्रयास में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार व्यक्ति उन वस्तुओं की प्राप्ति हेतु अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देता है जिन्हें वह सुखवर्धक मानता है; किन्तु दुर्भाग्यवश उसे सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों? कारण अत्यन्त स्पष्ट है। वह उस वस्तु की खोज में रत है जो वहाँ नहीं है। संसार के अपूर्ण, परिवर्तनशील और अनित्य पदार्थों के मध्य वह सुख की खोज कर रहा है। अतः अपूर्णता और विपर्यास बाह्य पदार्थों की प्रकृति ही है, अतएव उनके संसर्ग से परिणामतः मिश्रित अनुभव उद्भूत होते हैं। इसी कारण से मनुष्य के प्रयत्नों का परिणाम अपरिहार्यरूपेण भ्रान्ति, निराशा और सर्वथा असन्तोष होता है। जब कभी एक विषय से सन्तोष प्राप्त नहीं होता, मनुष्य सुख-प्राप्ति हेतु एक के बाद एक विषय का परीक्षण करता रहता है। एवंविध, जीवन-भर मनुष्य अनवरतरूपेण विषयों में सुख खोजने का प्रयास करता रहता है। सब दुःखों का अन्त करने वाले आनन्द की अनुभूति हेतु प्रयास में वह एक के बाद दूसरे विषय में उस आनन्द का अनुभव प्राप्त करने की चेष्टा करता है जिससे कदाचित् उसके सब दुःखों का अन्त हो जाये। उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अचिरेण ही उसे आभास होता है कि उसके अल्पकालीन जीवन का अन्त आ गया है। वह निज जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है।
महान् पुरुष जिन्होंने जीवन पर चिन्तन किया है और जो अन्तः एवं बाह्य प्रकृति की गहराई में उतरे हैं, उन्होंने कठोर आभ्यन्तर प्रयास द्वारा इस आत्यन्तिक सत्ता परमेश्वर, उस सत्त्व का साक्षात्कार किया है जिससे जीवन परिस्फुटित हुआ है। उन्होंने स्पष्ट एवं असन्दिग्ध शब्दों में कहा- "हे मानव! इस सीमित, नश्वर और अपूर्ण विश्व में तुम परिशुद्ध, पूर्ण सुख कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। स्वभाव से ही इसमें आत्यन्तिक सर्वातिरिक्त सुख निहित नहीं है। सुख और आनन्द की परमावस्था आपके अन्तर में ही प्राप्त की जा सकती है जिसका स्रोत शाश्वत नित्य आत्मा ही है। सब आनन्द और सुख भाव में निहित है।" इस कथन को और भी सुन्दर ढंग से इस प्रकार कहा जा सकता है-"आपकी प्रकृति ही यही है।" यह आपके भीतर निहित नहीं, प्रत्युत आप स्वयं ही आनन्द-स्वरूप हैं। आपका अन्तर्मन जीव, आपकी जीवात्मा, तत्त्वतः अनिर्वचनीय तथा आनन्द और शान्ति-स्वरूप है। उस आनन्द की साक्षात् जागृति हेतु पुनरन्वेषण जीवन का महान् कर्तव्य है। आपके जीवन का यह महान् उद्देश्य है। यही जीवन का लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति हेतु हमने इस भूलोक पर जन्म लिया है।
जीवन के सच्चे उद्देश्य की प्रतीति हेतु समुचित शिक्षण
युवकों को जीवन के अद्भुत उद्देश्य के प्रति अभिज्ञान कराना प्रत्येक माता-पिता, शिक्षक और वृद्ध का परम कर्तव्य है। जन्म से ही यदि प्रत्येक जीव को इस ज्ञान से अवगत कराया गया होता, तो कितनी ही खोज, संघर्ष और दुःखों से मुक्ति प्राप्त हो गयी होती। प्रारम्भ से ही जीवन सार्थक होता है। जीवन मात्र एक विषय से दूसरे विषय की ओर अविचारपूर्ण उड़ान नहीं है। जीवन तो अर्थ और महत्त्व से पूर्ण एक जिज्ञासा है। किन्तु प्रायः इस उद्देश्य का अभाव ही दृष्टिगत होता है, मनुष्य केवल अपने वृद्धजनों की पद्धति का यन्त्रवत् अन्धा अनुकरण करता है। "मेरे प्रपितामह ने ऐसा ही किया। मेरे दादा (पितामह) और पिता ने भी ऐसा ही किया; अतः मैं भी ऐसा ही करूँगा, क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे हैं" -इसे भेड़-चाल कहते हैं जो अनेकानेक जनों के जीवन का चित्रण करती है। जगत् के अन्य जनों का अनुभव इनका अनुभव होगा।
जो जनपद जीवन में निर्णय लेने तथा विवेक प्रयोग करने में असमर्थ हैं, उनके हाथ अन्ततः दुःख और निराशा ही लगती है। अतएव जीवन के अर्थ के प्रति जितना शीघ्र सजग होंगे, उतना ही अधिक प्रारम्भ से ही पूर्णता प्राप्त होगी। अन्यथा जीवन दिशाहीन यात्रा के समान लक्ष्य और पथ के ज्ञान से शून्य प्रधान पथ पर पग रखने के समान होगा। ऐसी परिस्थिति में आपसे यदि कोई प्रश्न करे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप उत्तर नहीं दे सकेंगे, लक्ष्य-ज्ञान बिना आप केवल जीवन-रूपी पथ पर चलने वाले मात्र प्रमादी पशु के समान होंगे। यह वास्तविक जीवन यापन नहीं है।
जीना जीवन नहीं
इस प्रकार आप जीवन-रूपी भँवर में फँस गये हैं और इसमें इतना अधिक उलझ गये हैं, इसके जाल में इतना गहराई में फँसे हैं कि सत्य जीवन-यापन की अपेक्षा मात्र जीविका-वृत्ति के क्रम में सर्वतः लीन रहते हैं। जीवन का स्थान जीविका-वृत्ति ले लेती है और स्वभावतः सच्चे उद्देश्य से च्युत होने के कारण आभ्यन्तर में एक अनिवार्य खोखलापन-सा आ जाता है और इस खोखलेपन (शून्यता) की पूर्ति आप बाह्य पदार्थों की प्राप्ति के प्रयास द्वारा करते हैं। किन्तु पदार्थ आन्तरिक सुख की अनुभूति प्रदान नहीं कर सकते। वे चिन्ता को जन्म देते हैं और अशान्ति तथा व्याकुलता का अनुभव देते हैं। सुख व्यक्ति के आन्तरिक जीवन की अवस्था है। यह मन और बुद्धि की अवस्था है। अतएव यह आन्तरिक दशा है। किसी भी प्रकार से वैभव से इसका सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि चिन्ता, अरक्षा और भय के कारण यहाँ मनोशान्ति में अनायास ही बाधा आ पड़ती है। अन्तःकरण में आध्यात्मिकता का वास्तव में दिवालिया ही हो गया है। सच्ची उपलब्धि की ओर जो भी प्रगति आपने की है, वह सच्ची सम्पत्ति है। अपने जीवन काल में आपने जितने भी पदार्थ संग्रहीत किये हैं, वे सब इहलोक में ही रह जायेंगे, वे नश्वर हैं। विश्व के सब पदार्थ मिल कर भी वास्तविक सन्तुष्टि प्रदान नहीं कर सकते; क्योंकि स्वभावतः ही वे ऐसा करने में असमर्थ हैं।
जीवन को विषयों से पूर्ण करने की आवश्यकता का सम्बन्ध अभाव से है। इसी अभाव की पूर्ति हेतु मानव द्रव्य संग्रह करता है। उसे ऐसी प्रतीति होती है मानो इन द्रव्यों के अभाव में वास्तविकसुख और आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती; किन्तु जब तक मनुष्य इन इच्छाओं का दास है, तब तक वह वस्तुतः सुखी नहीं हो सकता। दासता और सुख परस्पर अनुपमेय हैं। स्वतन्त्रता में सुख है, इच्छाओं के दास होने पर आप केवल पाशबद्ध प्राणी के समान होते हैं। ऐसी अवस्था में आप स्वतन्त्रता में सीमित आनन्द का अनुभव कैसे कर सकते हैं? सुख और परम सत्ता की आनन्दमयी अनुभूति की पूर्णता सब कामनाओं से परे है। आप निजात्मा को सर्वाकांक्षाओं से अतीत जानो ।
अन्धकार से प्रकाश की अवस्था आपकी वास्तविक अवस्था है। सम्पूर्णता आपकी सच्ची प्रवृत्ति है। उस 'पूर्णत्व' का साक्षात्कार करने पर आप सब प्रकार के अभाव के भाव से ऊपर उठ जाते हैं। तब आप न केवल इच्छाओं से ही मुक्त होंगे, अपने स्वभाव के इच्छा-रूपी तत्त्व से ही मुक्त हो जायेंगे। आप अनुभव करेंगे -"मैं सर्व सम्पन्न हूँ। मुझे कोई अभाव नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं 31 ^ prime prime आपके भीतर प्रचुरता का यह भाव निश्चयेन आनन्द है। यदि प्रचुरता का यह भाव आपके भीतर जागृत होता है, तो आप स्वामी हैं। तब और अधिक बन्धन नहीं रह जाता। इस संसार में आपको कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकता, आपको दास नहीं बना सकता। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करो और स्वयं को उस आनन्द तथा उस पराकाष्ठा से पूर्ण करो। यही आपके समक्ष गौरवपूर्ण कर्तव्य है। जीवन का प्रमुख उद्देश्य यही है।
भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य
आपको ज्ञात ही है कि विकारी, अपूर्ण विषय आपको अविकारी, पूर्ण अनुभूति प्रदान नहीं कर सकते। अब अपने जीवन को इस अविकारी, सर्व-सम्पूर्ण तथा इसी कारण से उत्तम तथा आनन्दमय तत्त्व का जिज्ञासु बनाने का प्रयास करो। आपको इस सत्य का सामना करना पड़ता है कि मनुष्य के रूप में आप परिवार एवं समाज के सदस्य होने के नाते दैनिक जीवन के कृत्यों से सर्वथा मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इच्छा अथवा अनिच्छा से हम यह कर्तव्य पूर्ण करते हैं; किन्तु जीवन के महानतम कर्तव्य आनन्द-प्राप्ति हेतु हम इनका सन्निधान कैसे कर सकते हैं?
भारतीय दर्शन के विषय में धूमिल परिचय प्राप्त करने वालों ने बुद्ध, निर्वाण, मायावाद और कर्मकाण्ड आदि के विषय में आश्चर्यजनक ही नहीं, प्रत्युत भ्रान्तिपूर्ण धारणा अपना ली है। उनके हृदयों पर अज्ञान-तिमिर का धूमिल आवरण छाया हुआ है जिससे इस धारणा का प्रादुर्भाव हुआ है कि भारतीय दर्शन दैवपरायण है, सर्वस्व मानो दैवाधीन है और कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं। वस्तुतः व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता था; क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार अन्तिम लक्ष्य शून्य ही होगा। इस विचार से तो मनुष्य स्वयं ही शून्य होगा; क्योंकि निर्वाण का अर्थ है-शून्य, अभाव! पतंजलि के सन्देश में कतिपय पुरुषों द्वारा उद्धृत इस अनुमान से बड़ी भ्रान्ति अन्यत्र दृष्टिगत नहीं हो सकती। स्पष्ट और अभ्रान्त शब्दों में भारतीय दर्शन यह घोषणा करता है कि मानव-जीवन का महान् लक्ष्य परमानन्द की प्राप्ति है। यह प्रमाणित करता है कि इस ब्रह्माण्ड में सभी प्राणी उसी आनन्द से उद्भूत हैं। आनन्द में ही उनकी सत्ता है, आनन्द से ही उनकी पुष्टि होती है और आनन्द-प्राप्ति ही उनका प्रयोजन है। अतः वस्तुतः यह अक्षय आनन्द ही महान् आत्यन्तिक सत्य एवं परम सत्ता है।
स्पष्ट है कि यह दैवपरक दर्शन नहीं है। इसमें अकर्मण्यता का समर्थन नहीं है। जब यह कहा जाता है कि परमावस्था शून्य है, जो इसका आशय है कि यह 'शून्य' ही है जिसका स्पष्टाक्षरों में वर्णन किया गया है। ऐसा करने के लिए वाणी अत्यन्त निर्बल और अक्षम है। यह शून्यता ही है जिसका मनुष्य की जीवात्मा ने अपने सापेक्ष, द्वैतावस्था में कदाचित् ज्ञान प्राप्त किया है अथवा कभी इसका अनुभव किया है। अतः मानव ने अपनी प्रमेयावस्था में सदा से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके अनुभव के दृष्टिकोण से यह अपेक्षाकृत सर्वतः नवीन और अद्वितीय अनुभव है। उस शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए मन और वचन से परे मौन ही एक विधि है।
भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का महान् लक्ष्य आनन्द की प्राप्ति है। हम कोई भी कर्म करें, हमें इस लक्ष्य को विस्मृत नहीं करना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति से हमारे सब अभाव दूर हो जाते हैं और हम ऐसी पूर्णता का अनुभव करते हैं जो सम्पूर्ण विश्व भी हमें प्रदान नहीं कर सकता और विश्व के सब पदार्थ उसे देने में अक्षम हैं। हमारे बाह्य जीवन का चित्रण उस आनन्दमय, प्रशान्त अनुभव के सर्वथा विपरीत है। किन्तु इस महान् प्राप्ति की जिज्ञासा में यदि कोई आगे बढ़ना चाहे, तो क्या पूर्वानुवर्तित अनुक्रम का उसे अवक्षेप करना होगा? क्या इस जीवन का त्याग करना होगा? क्या इसका परित्याग हो सकता है?
आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में समन्वय
प्राचीन एवं अर्वाचीन भारतीय सन्त आदर्शवादी तो हैं; किन्तु उनका आदर्शवाद वास्तविक है। यह अत्यन्त स्वाभाविक एवं सचेत वास्तविकता से युक्त है। आनन्द और शान्ति की खोज में अन्य जीवन के पूर्णत्व के प्रयत्न से संगति करनी है। सापेक्षिक स्तरों पर कार्य करने वाले जीवन के शारीरिक और मानसिक स्तरों की सच्चे आध्यात्मिक अस्तित्व से संगति करनी है। यह संगति आध्यात्मिक जीवन के कृत्यों में से एक है।
इस संगति को ध्यान में रखते हुए दो बातों का बोध आवश्यक है। प्रथमतः यह मन और बौद्धिक शक्तियाँ हमें साधन-स्वरूप में प्राप्त हैं; जब कि सामान्य जीवन में मनुष्य भौतिक शरीर एवं इन्द्रियों के संकेत पर कार्य करता है। वह स्वयं को इनसे पृथक् नहीं मानता। यह बोधगम्य प्रथम तत्त्व है। द्वितीयतः, मनुष्य मन इच्छाओं और तृष्णाओं के जाल में भी पूर्णतया फँसा हुआ है। किन्तु इन्द्रियों की अधीनता और मन की तृष्णाओं तथा इच्छाओं की दासता दुःखद एवं भ्रान्तिपूर्ण अवधारणा है। मन और इन्द्रियों को मात्र अनन्त विषय-वासनाओं तथा भौतिक सुखों की आसक्ति का साधन मान लेना कुटिल मति है। महान् लक्ष्य की प्राप्ति को समीप लाने के लिए आपको यह साधन प्रदान किये गये हैं। इसी उद्देश्य से इनका उपयोग करना चाहिए। ऋषियों का यही महोपदेश है कि सामाजिक प्राणी तथा समाज का सदस्य होने के नाते मनुष्य को एक सच्चे परिश्रमी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह श्रम प्राणिमात्र की निःस्वार्थ सेवा का अपर स्वरूप भी धारण कर सकता है।
अनुभव इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि मनुष्य की शक्तियों के यत्न से अन्य जनों को प्रदत्त महान् उपकार श्रम के उच्चतम स्वरूप से उद्भूत होता है। व्यावहारिक जीवन में मनुष्य को अपने परिवार, निकट सम्बन्धी तथा मित्रों आदि का ध्यान रखना चाहिए तथा उनकी देख-रेख सतत रूप से करते रहनी चाहिए। व्यष्टि-रूप में उसे अपने शरीर तथा मन के प्रति समुचितरूपेण सावधान रहना चाहिए। एवंविध, सेवा तथा परोपकार का जीवन व्यतीत करने से आपकी पूर्णता बनी रहती है। ऐसा करने से आप आध्यात्मिक जीवन से पृथक् नहीं होते। जब आपका जीवन सत्य और ईमान के नियमों पर आधारित होता है, तब जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष आपके आध्यात्मिक विश्लेषण के आन्तरिक जीवन की प्रगति में विघ्न-रूप कदापि नहीं रह जाता।
बाह्य जीवन में जिस प्रकार सम्यक् कर्म का अनुसरण अनिवार्य है, उसी प्रकार मानसिक जीवन में भी सम्यक् चिन्तन होना चाहिए। इन्द्रियों के आकर्षण से जो विचार अंकित होते हैं, वे अयथार्थ हैं। धर्मानुसार कार्य करने वाले विचार सत्य हुआ करते हैं। अतएव, विचारों का चिन्तन करो। पवित्र विचारों का चिन्तन करो।
निःस्वार्थ भावों का चिन्तन करो। भूल जाओ - "मुझे क्या प्राप्ति होगी? मुझे क्या मिलेगा? जीवन को सम्पूर्ण करने के लिए मैं कौन-कौन-से सुख-भोगों की अवाप्ति करूँगा?" विपरीत सोचो - "मेरे द्वारा किस प्रकार अन्य जनों का कल्याण हो सकता है? मैं दूसरों की प्रसन्नता में संवृद्धि कैसे ला सकता हूँ? दूसरों का दुःख कैसे कम कर सकता हूँ? इस ब्रह्माण्ड के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हेतु बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? सत्य क्या है? असत्य क्या है? शाश्वत क्या है? अन्तिम लक्ष्य क्या है और क्षणिक जीवन से सम्बद्ध कौन-सा तत्त्व है?" एवंविध, बुद्धि सदा वास्तविक सत्य, आनन्दप्रद और सुखकर सत्य और मिथ्या, शाश्वत और गमनशील का सदा विवेक रखे। इस विश्व परिज्ञान, भौतिक पदार्थों की प्रकृति का ज्ञान तथा आत्म-निरीक्षण करना ही बुद्धि का उचित उपयोग है। इस प्रकार आपको ज्ञात होगा कि विचार किस प्रकार कार्य करते हैं, इच्छाएँ कैसे प्रबल होती हैं और इन्द्रियाँ किस प्रकार आपकी वंचना करती हैं और विचारों तथा इन्द्रियों को वशीभूत कैसे किया जाये। विवेक जागृत करो। इसे पथ-प्रदर्शन का कार्य करने दो। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तो यह है कि आध्यात्मिक जीवन आपको लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करे।
समस्याएँ जब कभी भी आपके समक्ष आ खड़ी हों, स्वयं से यह प्रश्न कीजिए-"क्या यह मुझे अन्तिम लक्ष्य के निकट पहुँचायेगी अथवा यह मेरे जीवन की सुन्दर लक्ष्य-पूर्ति में बाधा-रूप है?" यह विषय विशेष होना चाहिए। यदि कोई पदार्थ अथवा कर्म आपको वैषयिक जीवन की ओर आकृष्ट करे, तो उन्हें स्वीकार मत कीजिए; किन्तु यदि यह परम लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करे, तो इसे स्वीकार कर लें। इस प्रकार शरीर और मन से समुचित कार्य लेना चाहिए और व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक पक्षों को सबसे महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्नत करने के लिए व्यावहारिक रूप में शिक्षित करना चाहिए।
सभी पक्षों का समन्वय होने पर बाह्य जीवन के रूप अथवा संस्कार अधिक महत्त्व नहीं रखते। यदि आप चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक ही बने रहें। शिक्षक हैं, तो शिक्षक ही बने रहें। व्यापारी हैं, तो व्यापारी बने रहें; किन्तु व्यापारी सच्चा बनना चाहिए। चिकित्सक को दयालु होना चाहिए। मात्र शुल्क-आकर्षण ही नहीं होना चाहिए। कर्म के नियमों का अभ्यास करने पर ही एक सिपाही भी अपने ऊपरि जनों के आदेश पर कार्य करता हुआ एक सच्चा अध्यात्म-परायण हो सकता है। यदि वह अनासक्त है, तो उसका जीवन उसे लक्ष्य के समीप ले जायेगा। अतः धर्माचरण आपका पथ-प्रदर्शक बना रहे।
गुणों का अभ्यास
सदाचार में किन-किन गुणों का समावेश है? उत्तर सत्य के स्वरूप में ही निहित है। सत्य-परायण बन कर आप भगवद्-साक्षात्कार शीघ्र कर सकते हैं। किन्तु यदि जीवन असत्यता से परिपूर्ण हो, तो भगवान् कोसों दूर हैं। तब सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि उस दशा में व्यक्ति स्वयं को आनन्दमय-स्रोत से पृथक् कर लेता है। उससे सम्बन्ध विच्छेद कर व्यक्ति को सम्पूर्ण पृथ्वी भी सुख प्रदान नहीं कर सकती। स्वभाव से ही, शान्ति और सुख उसके जीवन में नहीं आ सकते जो सच्चाई पर नहीं चलते। अतः धर्मपरायणता जीवन में सत्य के नियमों का अनुष्ठान है। इसका प्रवास आपकी आभ्यन्तर वास्तविक सत्य दिव्य प्रकृति में है।
दया, सबसे प्रेम, प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव सत्य का अभ्यास है। आपकी वास्तविक प्रकृति इन्हीं गुणों से युक्त है। यह आपके उच्चतर आध्यात्मिक पक्ष का निर्माण करते हैं। अतः अपने सम्बन्धियों के लिए, माता-पिता, बालक, बन्धु, सखा, मित्र एवं सहवासियों के लिए कृपापूर्ण सम्मान का भाव रखो। जीवन में इस अभ्यास के बिना आध्यात्मिक आनन्द की प्राप्ति असम्भव है। कटु वाणी, कटु वचन, क्रोध का आवेश तथा उत्तेजना जिनसे दूसरे के भावों को कष्ट पहुँचता है, प्रयोग नहीं करने चाहिए। दूसरों के जीवन में प्रसन्नता का संवर्धन करने से सुख की अनुभूति होती है। यह उन्हें ही प्राप्त होता है जो प्रेम, दया और कृपा के केन्द्र हैं तथा जो ईश्वर के प्राणियों को दुःखी करने का विचार भी मन में नहीं आने देते।
सब कर्मों के पीछे उद्देश्य नितान्त पावन होना चाहिए। विचार तथा उद्देश्य दोनों ही भद्र, उत्कृष्ट एवं पवित्र होने चाहिए। अत्यन्त शुचिता का स्तर रखने वाला मनुष्य पवित्र वाणी और कर्म का भागी होता है। अपवित्र विचार अथवा उद्देश्य, लोभ, काम अथवा क्रोध से समन्वित अपवित्र विचार अथवा उद्देश्य तत्काल ही कर्म को कलंकित कर देता है। लोभ तो एक अग्नि है जिसमें आहुति डालने से वह और अधिक प्रज्वलित होती है।
सन्तुष्ट व्यक्ति सदा सजग रहता है और लोभी विचार को पहचानता है जिसे वह अपने मन से विन्यस्त कर देता है। सुख उसे ही प्राप्त होता है जो सन्तुष्ट है। ऐसे सन्तुष्ट व्यक्ति को किंचिद् रुचिकर पदार्थ प्राप्त हो जायें, तो वह प्रसन्न होता है और न प्राप्त हों, तो भी वह प्रसन्न ही है। वह इस भ्रम में नहीं पड़ता कि पदार्थ सुखदायी हैं। आप उस अनुभव को सुखद कैसे कह सकते हैं जो अपनी पूर्ति हेतु बाह्य पदार्थों पर निर्भर है? क्योंकि पदार्थ की क्षति (विषय-लोप) के साथ ही वह अनुभव भी समाप्त हो जाता है। और भी, जिस प्रकार पदार्थ विकारी होते हैं तथा विविध अनुभव भी परिवर्तनशील होते हैं, सब पदार्थ परिवर्तनशील हैं और यहाँ आपका अधिष्ठान भी क्षणिक है। अतः विश्व में सब पदार्थों से आपका सम्बन्ध अनित्य है।
मेरे गुरुदेव विनोद करते हैं-"इस संसार की सभी अनिश्चितताओं और असुरक्षा के मध्य केवल एक वस्तु निश्चित है कि आपको जाना है, आप यहाँ नहीं रह सकते। यह तो एक स्वल्प नाटक है जिसका आप अभिनय कर रहे हैं। अव्यक्तावस्था से आप इस व्यक्त, सदेहावस्था में पहुँचे हैं। प्रत्येक क्षण आपके जीवन-काल को अल्पतर कर रहा है। वह समय कितना है, किसी को ज्ञान नहीं। प्रत्येक जन्म-दिवस जिसे आप निमन्त्रण-पत्र, केक और मोमबत्तियों (दीपिकाओं) के साथ अतीव हर्षोल्लास से मनाते हैं, वह आपके जीवन काल से आपको एक वर्ष दूर ले जाता है। अचिरेण ही निर्धारित समय का अन्त आना है। पुनः उस अव्यक्तावस्था में आपका पुनरावर्तन होगा जहाँ आप देह-मुक्त हो जायेंगे, आपका कोई व्यक्तित्व नहीं रहेगा, कोई नाम नहीं रहेगा। आपको जाना ही है।"
सुख-शान्ति हेतु परिवर्तनशील तथा नश्वर पदार्थों पर निर्भर होने से बढ़ कर और क्या मूर्खता एवं अविचारता हो सकती है। सुख बाहर से नहीं आता। जिसे यह ज्ञान है कि सुख की प्राप्ति भीतर से ही होती है, वह सन्तोष-नियम के प्राचीन आदर्श का अनुसरण करता है। वह स्वर्ण नियम है। जो वस्तु यथार्थतः आपकी नहीं, उसके लिए लालसा मत करो। जिसे प्रकृति की ओर से रूप का सौन्दर्य प्राप्त नहीं हुआ, उसे दूसरे के रूप के सौन्दर्य पर ईर्ष्यावलोकन नहीं करना चाहिए। भगवान् ने ही उसे वह विशेष मुखाकृति प्रदान की है। मन में जब यह विचार उदित हो कि 'मैं अमुक व्यक्ति की भाँति क्यों नहीं बनूँ? जो उसके पास है, वह मेरे पास क्यों न हो', तब मन अशान्त हो उठता है। मानसिक शान्ति के बिना सुख कहाँ?
जन-जन के दैनिक जीवन में यदि तृष्णा के विरुद्ध इस नियम का अनुष्ठान होने लगे तो सब विषाद, कलह, घृणा और हिंसा समाप्त हो जायें। राष्ट्रीय स्तर पर भी कलह का कारण इस नियम का उल्लंघन है। प्रत्येक पुरुष अपने सहवासी (पड़ोसी) की जेब में हाथ डालना चाहता है। इस प्रकार से पुरुष यदि अविवेकी हों, तो महान् देशों से हिंसा के सशपथ त्याग की हम कैसे आशा कर सकते हैं। धरती पर महान् प्रज्ञावान् और उच्चतम विज्ञानिकों से सम्पन्न राज्य इन दोषों के कारण पाश में बंध गये हैं।
धर्म का मूल तत्त्व आपको सब मनुष्यों के लिए सुख-साधन बताता है। अतएव आपका जीवन सत्य, शुचिता एवं सार्वभौमिक प्रेम के उच्चतम नीति-नियमों पर आधारित होना चाहिए। यह अनिवार्य नहीं है कि इन नियमों के अनुष्ठान हेतु परिवार त्याग कर किसी गुहा, हिमालय, वन अथवा किसी मठ या आश्रम में वास किया जाये। इन नियमों का पालन करने पर आपका अपना निवास भी, चाहे वह झोपड़ी भी हो, आनन्द-स्वरूप स्वर्ग बन जायेगा। इसका स्वरूप किसी मठ अथवा विहार से भी कहीं अधिक सुन्दर होगा। मात्र इसके द्वार में दया और करुणा पर आधारित आपका जीवन, धर्म और न्याय-रूपी आदर्श के उत्कृष्टतम स्तर की ओर उन्नत होगा।
यह नियमित अनुष्ठान आपके भीतर सत्य की अनवरत जिज्ञासा को पुष्ट करेगा। प्रत्येक नव-दिवस जीवन के परम उद्देश्य की गहनतर आभ्यन्तर जागृति को ले कर आयेगा। जीवन अत्यन्त अमोघ है। ऐसा कहें- "मैं यहाँ आनन्द की परमावस्था का साक्षात्कार करने एवं उत्कृष्ट आनन्द की अनुभूति करने आया हूँ। आत्यन्तिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुझे यह मानव-जन्म और मनुष्य-जन्म-रूप में अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है।"
अब तो अवसर हाथ में है। किसे ज्ञात है कि सर्वोच्च नियमों के प्रति अभीप्सा और आदान की यह उत्कृष्ट स्थिति कब तक रहेगी, कौन जानता है कि आदर्श के प्रति उत्सुकता की अवस्था निरन्तर बनी रहेगी? अतः अभी समय है-जीवन के सच्चे उद्देश्य के साक्षात्कार हेतु यत्न करने का समय अभी है। यही समय है, सर्वोच्च आनन्द तथा साक्षात्कार के अनूठे आनन्द की प्राप्ति का यही समय है।
७. स्वास्थ्य और समृद्धि के नियम
प्रिय अमर आत्मन्! शाश्वत ज्योतिस्वरूप परमात्मा की गरिमामयी रश्मियो! आपको नमस्कार एवं परम सत्ता को कोटिशः प्रणाम!
भारत के महर्षियों के ज्ञान में से कतिपय शब्द आपके समक्ष उस विषय पर कहूँगा जो यद्यपि आपके अस्तित्व का नश्वर अंश हैं, असत्य हैं, आपकी सत्ता का परम सत्य नहीं हैं, तथापि निजी रूप में महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये परब्रह्म के साक्षात्कार का साधन स्वरूप हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि, जीवन के सच्चे और चिरन्तन उद्देश्य 'आप कौन हैं' का बोध प्राप्त करने के लिए सहायी और साधन तत्त्व है।
'आप कौन हैं' - इस सत्य की प्रतीति होते ही आप मुक्त हो जाते हैं। आप इहलौकिक सत्ता, देह-मन के कष्टप्रद संकुचित ससीम बन्धन, इच्छा, वासना, भय तथा मूल अविद्या के पाश से सदा-सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं जिनके कारण आप अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल गये हैं और भ्रमवश स्वयं को वह मान बैठे हैं जो आप नहीं हैं। आप तो सदा अमर हैं, जन्म-मरण रहित हैं, अव्यय हैं, अविकारी हैं। आप सदा अमर ही रहेंगे; क्योंकि यह शाश्वत सत्य है, आपके अस्तित्व की वास्तविकता है और इस क्षण भी आपके अस्तित्व का यह उज्ज्वल सत्य है। आप इस समय नित्य स्वरूप हैं। इसी क्षण भी आप असीम आनन्द तथा अपरिमेय शान्ति का सत्त्व हैं। अपनी सम्पूर्णता, अखण्डता, निर्दोष-निष्कलंक वैभव (तेज) से सम्पन्न आप वही हैं, परब्रह्म हैं। इसका साक्षात्कार करना ही इस पार्थिव जीवन का महान् उद्देश्य है।
मनुष्य की सदेहावस्था के सम्बन्ध में हमारे प्राचीन सन्त अपनी ही प्रकार के सत्यवादी थे। उन्हें मानव की इस गरिमामयी आभ्यन्तर प्रकृति की साक्षात् ज्योति का आभास था और वे इस रहस्य के उन्मीलन के असीम आनन्द से परिपूर्ण थे।
एवंविध, शाश्वत सत्यों के उद्गारों से युक्त पुरातन ज्ञान के चार महान् कोष्ठ-वेद-चतुष्टय के साथ ही हमारे पास आयुर्वेद नाम से एक पंचम वेद भी है। यह शब्द अतीव अर्थपूर्ण है। आयु का अर्थ है- आपका यहाँ 'जीवन काल' और वेद का अर्थ है-'ज्ञान'! अतः आयुर्वेद का अर्थ हुआ जीवन विज्ञान !
मानव-जीवन का विज्ञान, इस जीवन की रक्षा कैसे करें, सुखपूर्वक कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहे, इसका रहस्योन्मीलन आयुर्वेद करता है। अन्य वेदों की आध्यात्मिक निधि के गर्भ से यह रहस्य भारतीय पद्धति के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग को प्रदान किया गया है। एवंविध, आयुर्वेद चार वेदों में निहित मूल तत्त्वों पर आधारित है।
भारतीय आचार्यों की मानवेक्षणा
भारतीय विचारधारा भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित होती है और इस तथ्य को लक्षित करती है कि आपका प्रथम और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कर्म आत्मज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि आप सब विद्याओं के मूल तत्त्व रूप हैं। सर्वप्रथम, वस्तुओं का दर्शन करने के लिए द्रष्टा और विषयों पर ध्यान करने के लिए दृष्टिगोचर विषयावलोकन हेतु ध्याता होना चाहिए। यदि किंचिद् ज्ञान है, तो उसकी प्राप्ति हेतु ज्ञाता चाहिए। अतएव इस ब्रह्माण्ड का आधार, सर्वविद्याओं का मूल, ज्ञाता के प्रतिज्ञान, आपका निजी आत्म-विज्ञान सर्वप्रथम विन्यस्त किया गया। तदुपरान्त अन्य ज्ञान की चिन्ता करें जो आपसे विलक्षण हो।
मनुष्य की सत्यता के प्रति पुरातन ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह जीव स्थूल अथवा पार्थिव नहीं है। विकार, परिवर्तन, विनाश और क्षय से युक्त उसके व्यक्तित्व के स्थूल, भौतिक जगत् के अंश (शरीर) केवल अनुबन्ध कोप अथवा आवरण थे जिन्होंने उसके नित्य ज्योति स्वरूप आत्मा को मानो अवगुण्ठित कर लिया। बन्धनयुक्त कर दिया। अपने इस स्वरूप में वे उस जीव के बाह्य अंश बने, अनिवार्य नहीं और आध्यात्मिक जीवात्मा तो आभ्यन्तर में सात्त्विक चैतन्य था।
इस दिव्य चेतना के समीपतम मन का निवास है और भारतीय आचार्यों के अनुसार मन, भौतिक शरीर की ही भाँति स्थूल है। जहाँ तक मन का आत्मा के साथ सम्बन्ध है, वे मन को शरीर से उच्चतर स्थान नहीं देते। हाड़-मांस के शरीर अथवा लोष्ठ-पिण्ड की भाँति ही मन का आत्मा के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है। मन भी अत्यन्त सूक्ष्म द्रव्य है। यह स्थूल विषय है। आध्यात्मिक चेतना ही यथार्थतः दिव्य प्रकृति की है और सापेक्षतः मन सूक्ष्म द्रव्य है, शरीर स्थूलतर द्रव्य है और बाह्य स्वरूप स्थूलतम है।
जीवात्मा के सम्बन्ध में भारतीय आचार्यों का एकमत है कि शरीर की अवस्थाएँ अन्तस्तम आत्मा और शरीर को आवृत किये हुए विविध कोषों की आन्तरिक क्रीड़ा पर आधारित हैं। यदि मन, बुद्धि, भाव, भावनाओं की विराट् शक्ति एवं शरीर के प्रत्येक छिद्र एवं नाड़ी-तन्तु द्वारा आत्म-शक्ति को अप्रतिबाधित क्रीड़ा का अवसर दिया जाये तो शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। यदि आत्म-शक्ति की इस स्वतन्त्र क्रीड़ा का अवरोध करें अथवा इसे भ्रंश कर दें तो अवगुण्ठित कोषों में रुग्णावस्था का प्रादुर्भाव होने लगता है।
यह अवरोध दो प्रकार से आता है। प्रथमतः आपकी चेतना पर अज्ञान का ऐसा आवरण पड़ जाता है कि आप अपने जीवन के आध्यात्मिक स्रोत ईश्वर के साथ अपने शाश्वत सम्बन्ध को पूर्णतया विस्मृत कर देते हैं। यदि मन और बुद्धि के कामनामय तथा शरीर की इन्द्रियों के वासनामय व्यक्तित्व में आप पूर्णतः आसक्त हो जाते हैं, उससे अभिभूत अथवा जालबद्ध हो जाते हैं, तब परमात्मा के साथ आपकी संयोग की कड़ी टूट जाती है और आप जीवन में पूर्णत्व एवं कल्याण-प्राचुर्य प्राप्त नहीं कर सकते; क्योंकि सर्व कल्याण, सर्व प्राचुर्य आपके जीवन के अनन्त स्रोत से प्रवाहित होता है। परमेश्वर से ही हम अपनी प्रकृति का सर्वपक्षीय हित स्व प्रकृति के सर्व स्तरों में प्राप्त करते हैं और यदि हम स्वयं को उस मूल से विलग कर लेते हैं, तो वृक्ष से कट कर लटकती हुई शाखा की भाँति हम विनाश को प्राप्त होते हैं। जीवन के मूल-स्रोत से वियुक्त हो कर जीवन रोग, व्याधि, दुर्बलता, अपूर्णता, दुःख एवं शोक का भागी बन जाता है।
इसी प्रकार शरीर तथा शारीरिक शक्ति, पार्थिव शरीर के भीतर ही सूक्ष्म प्राण के रूप में अभिव्यक्त होने वाली अन्तः प्राण-शक्ति और हमारे निजी विचारों तथा संवेगों की शक्ति के दुरुपयोग द्वारा यदि हम उन्हें इतना स्थूल बना देते हैं और दिव्य प्रकृति की अभिव्यक्ति के प्रति असंगत कर देते हैं तो यह स्तर हमारी आत्म-शक्ति और कल्याणकारी प्रभाव से वियुक्त होने के कारण रुग्ण होने लगते हैं। अतः सम्पूर्ण आयुर्वेद इस सिद्धान्त पर विरचित है कि वह साधन जो शुद्ध और सम्पूर्ण है, जो सूक्ष्मावस्था में है और दिव्य प्रकृति को स्वयं ही सहज प्रस्फुटन का आदेश देता है वह स्वास्थ्यवर्धक है और इस प्रकार निज अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर विविध शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा यह स्वतन्त्र क्रीड़ा दूषित कर दी जाती है, तब हमारा पूर्ण जीवन अस्वस्थता एवं दुःख की ओर प्रवृत्त होने लगता है। आयुर्वेद के सिद्धान्त के अनुसार दुःख, जीव को संशुद्ध करने और निर्मल सूक्ष्म अवस्था की प्राप्ति हेतु स्मारक है। यदि रोग और अस्वस्थता का पाठ तत्काल ही सीख कर वह अपने स्वभाव को परिणत करके जीवन की भूल को शरीर तथा मन से सुधार लेता है तो मानव देह की मौलिक स्वाभाविक अवस्था एक बार पुनः सूक्ष्म हो उठेगी।
स्व अस्तित्व के स्तर-चतुष्टय से अब आप अवगत हो चुके हैं। आपके भीतर ही आपका सात्त्विक स्वाभाविक जीव रूप है और सच्चिदानन्द, शान्ति, शुद्ध और पूर्ण स्वरूप आपका जीवात्मा शरीर के मध्य में अधिष्ठित है।
द्वितीयतः आपके सत् स्वरूप के सर्वतः मनोमय-कोष है जहाँ बौद्धिक, मानसिक एवं संवेगात्मक क्रियाओं का जन्म होता है। इससे अग्रिम, बाहर की ओर प्राणमय-कोष है जिसमें शरीर को संचालित करने तथा इसे जीवित रखने की प्राणभूत शक्ति निहित है। तत्पश्चात् अस्थि, मांसपेशियों, नाड़ी, संयोजक तन्तु एवं भौतिक शरीर का निर्माण करने वाले अनेक अंगों से युक्त आपका बाह्य शरीर है। मन, प्राण और शरीर के तीन स्तरों में मनुष्य को पवित्रता और परिष्कृति का एक विशेष स्तर रखना पड़ता है।
स्वस्थ रहने के लिए भोजन कैसा हो?
प्रधानतः आहार के द्वारा शरीर की परिष्कृति, शरीर की शुद्धि निश्चित है। उचित समय पर युक्ताहार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हितकर है। एक महान् ऋषि आत्रेय hat 7 कहा- "उचित आहार परिमित मात्रा में, उचित समय पर, उचित ढंग से ग्रहण किये जाने पर व्यक्ति के स्वास्थ्य का निश्चय कराता है।" उचित आहार से उनका अभिप्राय क्या था? सात्त्विक आहार, शुद्ध आहार तथा शुद्ध रूप में उचित समय पर लिया गया आहार ही उचित (युक्त) आहार है। सभी स्वास्थ्य विभाग आपको बतायेंगे कि दिवस की कतिपय वेला-विशेष में हमारे शरीर की शक्ति उदात्त अवस्था में होती है और उस समय ग्रहण किया गया भोजन हितकर होता है और जब शारीरिक शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, तो आहार नहीं लेना चाहिए। उत्तेजना अथवा चित्तक्षोभ आदि विकार की अवस्था में भोजन नहीं लेना चाहिए। समग्ररूपेण ग्रहण करने का अभिप्राय है-भक्ति-भाव से, प्रभु-मग्न हो कर, शनैः शनैः मौन-भाव से और भली प्रकार चबा कर तथा सर्वतोपरि, सन्तुलित मात्रा में लिया गया आहार। इन नियमों का पूर्णतया पालन करने पर आहार शरीर को शुद्ध करने, इसका शक्ति-संवर्धन करने तथा परिष्कृत अवस्था में रखने में सहायी होता है; क्योंकि भारत में आयुर्वेद के विज्ञान के अनुसार आहार की नितान्त अनुपम व्याख्या है।
भोजन 'अन्न' कहलाता है। प्रत्येक भक्ष्य पदार्थ 'अन्न' है। अन्न के दो अर्थ है-प्रथम भक्षण अथवा भोग (अद्यते इति अन्नम्) और द्वितीय समान रूप से ही प्रमाणित अर्थ है-वह जो उपभोग (क्षय) करता है (अत्ति इति अन्नम्) । यह द्वितीयार्थ आयुर्वेद में समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। भक्ष्य पदार्थ आहार है। आहार भक्षक भी है। आप यदि इस पर विचार करें तो प्रतीत होगा कि आहार शब्द का द्विगुणित अर्थ है। सन्तुलित आहार जीवनदायी है; असन्तुलित आहार स्वास्थ्य एवं अन्ततः जीवन को नष्ट करने वाला होता है।
नियम और विधान का निरूपण करने पर ज्ञात होता है कि मनुष्य की सर्वोत्तम शक्तियों को क्षीण करने वाला आहार ही है; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की प्रतिदिन एव दिन-प्रतिदिन, मृत्यु-दिवस पर्यन्त की शक्ति आहार, पाचन, समीकरण एवं मलोत्सर्ग आदि में क्षय होती है। प्रतिदिन शरीर में उत्पन्न होने वाली पचासी से नब्बे प्रतिशत शक्ति पाचन, समीकरण एवं आहरण की प्रक्रिया में नष्ट होती है। अतः आप देखते हैं कि आहार किस प्रकार से आपकी प्राण-शक्ति, आपकी जीवन-शक्ति का भक्षण करता है।
जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सम्पूर्ण रक्त-संचार आमाशय की ओर केन्द्रित हो जाता है और शरीर की सम्पूर्ण व्यवस्था को पचाने एवं शरीर में विलय करने की क्रिया करनी पड़ती है। जैसे शारीरिक व्यवस्था दिन-प्रतिदिन शैशव से यौवन, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था पर्यन्त यही क्रिया करती है। एक समय ऐसा आता है, जब भोजन ग्रहण करना असम्भव हो जाता है; क्योंकि इन शक्तियों के उपभोक्ता शरीर में पचाने की शक्ति नहीं रह जाती और व्यक्ति सोचता है कि असंख्य टन भोजन को पचाने में उसका जीवन व्यतीत हो गया है। कदाचित् बाल्यावस्था से अब तक ग्रहण किया हुआ भोजन यदि संचित किया जाता तो एक बड़ा धान्यागार अथवा भण्डार भर जाता। इस प्रकार अन्न ही भक्ष्य है तथा अन्न ही आपके जीवन के माध्यम से इसे ग्रहण करता और भक्षण करता है।
आयुर्वेद के विज्ञाता के अनुसार स्वास्थ्य के मौलिक नियम सन्तुलित आहार की श्लाघा हेतु यह उदार दृष्टिकोण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। समुचित रूपेण, नियमित समय पर युक्ताहार स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी है। शक्ति में परिणत होने वाला यह आहार समस्त शरीर में शारीरिक शक्ति अन्तः प्राण के रूप में अभिव्यक्त होता है। प्राण का असत्प्रयोग होने पर जीवन नष्ट हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। व्यष्टि में प्राण किस रूप में विद्यमान है? यह व्यष्टि में सम्भोग-शक्ति, प्राण-शक्ति तथा जीवन-शक्ति के रूप में विराजमान है और इस जीवन-शक्ति का कुप्रयोग अथवा अपव्यय स्वास्थ्य के कल्याण और जीवन का ही सबसे बड़ा नाशक है। एक महान् उक्ति है- "प्राण-शक्ति की रक्षा जीवन है और प्राण-शक्ति का हास विनाश है।"
आत्म-संयम और जीवन-शक्ति की रक्षा
भारतीय चिकित्सक जीवन-शक्ति की रक्षा पर अत्यन्त बल देते हैं। सम्भोग में सन्तुलन एक युक्ति है जिसका उपदेश वे पुनः पुनः सदा से करते आये हैं। रोगी के निरीक्षण तथा उसके भोजन आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करके आदेश देने के उपरान्त चिकित्सक इस बात पर बल देता है कि चिकित्सा-काल पर्यन्त रोगी को सहवास नहीं करना चाहिए। पूर्णतया स्वस्थ होने के उपरान्त ही चिकित्सक उसे सामान्य लौकिक जीवन यापन करने का आदेश देने के लिए विचार करता है और आयुर्वेद के अनुसार सामान्य भौतिक जीवन आसक्ति नहीं है। ऐसी धारणा बन गया है कि सामान्य लौकिक जीवन दो तथ्यों से चित्रित होता है, वे हैं-संयम और सन्तुलन। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त आयुर्वेदीय ज्ञान जीवन-शक्ति, प्राण-शक्ति को सुरक्षित रखने के मूल सिद्धान्त पर आधारित है। इसके बिना सुस्वास्थ्य असम्भव है। आप यदि इस सिद्धान्त की उपेक्षा करें तो विश्व-भर के समस्त औषध-गृह आपको स्वस्थ नहीं कर सकते, इस विश्व के सर्व चिकित्सक और शल्य चिकित्सक आपको कुशलता, शक्ति और प्राण-शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। यह ऐसी वस्तु है जो आपके भीतर ही है और आपको उसकी रक्षा करनी है और यदि आप ही भोगासक्त हैं तो अन्य जन आपको यह नहीं दे सकते; क्योंकि यह देय बाह्य पदार्थ नहीं है। यह बोतलों, गुल्लिकाओं, चूर्ण अथवा पेय पदार्थों से प्राप्य नहीं है। ऐसा असम्भव है। यह आपके जीवन का ही अंश है और जीवन में संरक्षण अथवा सन्तुलन द्वारा इसकी संवृद्धि हो सकती है।
आयुर्वेद का विज्ञान इसी एक सिद्धान्त पर आधारित है और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षार्थी को प्रारम्भ से ही आत्म-संयम तथा प्राण-शक्ति की सुरक्षा का आदेश दिया जाता है। उसके अभाव में अथवा उसके दूषित होने पर प्राणमय-कोष अनियन्त्रित हो जाता है। जिस प्रकार एक भूल आपके शरीर को दूषित करके इसे अशुद्ध और स्थूल बना देती है, उसी प्रकार प्राण-शक्ति में एक भूल आपके प्राणमय-कोष को दूषित कर देती है। आहार से शरीर जो शक्ति ग्रहण करता है, प्राण-शक्ति उसका तत्त्व है, सार है। उसकी असुरक्षा पर प्राणिक कोष विक्षिप्त हो कर सन्तुलन खो देता है और शरीर में प्राण अव्यवस्थित रूप में संचार करने लगता है। सभी रोग आन्तरिक प्राण की विक्षिप्तावस्था के कारण उत्पन्न होते हैं।
और यदि मन आपकी आन्तरिक सम्पूर्णता की अभिव्यक्ति का क्षेत्र बनने की अपेक्षा विचारों, संवेगों एवं भावनाओं का क्रीड़ा-क्षेत्र बन जाता है जो सर्वथा अधर्मवृत, पाशविक एवं स्थूल बनने की अपेक्षा विचारों, संवेगों एवं भावनाओं का क्रीड़ा-क्षेत्र बन जाता है जो सर्वदा अधर्मवृत, पाशविक एवं स्थूल तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या से युक्त होते हैं तो शरीर मन की इस विचारपूर्ण अवस्था में नीरोग नहीं रह सकता।
शरीर और मन-व्याधि और अधिव्याधि
मन रुग्ण और अस्वस्थ हो, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। शरीर में भोजन से बना रक्त विषाक्त हो जायेगा। मन में भरे हुए भाव यदि स्थूल, अपवित्र और विनाशी प्रकृति के हों, सात्त्विक न हों, आध्यात्मिक प्रकृति के न हो कर शारीरिक प्रकृति के स्थूल हों तो शरीर भोजन से अधिकतम शक्ति सँजोने में अक्षम होगा। विषयासक्ति और आवेशपूर्ण भाव जैसे-घृणा, ईर्ष्या और हिंसा, सच्चे अस्तित्व की अभिव्यक्ति हेतु मन को साधन के रूप में सर्वथा अक्षम बना देती हैं; क्योंकि ऐसा मन रोग के अंकुरों का क्षेत्र बन जाता है। ऐसा मन आन्तरिक अवस्था रुग्णावस्था को जन्म देने के लिए समृद्ध स्रोत और रम्य-स्थल बन जाता है। आयुर्वेदिक आचार्यों ने इस सत्य का उन्मीलन तीन सहस्र से अधिक वर्ष पूर्व किया था। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने अकस्मात् ही ऐसा अनुभव किया है कि चिकित्सालयों में पचास से अस्सी प्रतिशत से अधिक शारीरिक रोगों का मूल कारण मन में है जो शरीर में अभिव्यक्त होते हैं।
कतिपय यूरोपियन मनोवैज्ञानिकों ने कुछ समय पूर्व ही यह अन्वेषण तथा अनुभव किया है कि शरीर में होने वाले सभी रोग मन से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ज्ञान का मूल स्रोत आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक आचार्यों ने कहा कि जब तक मनोभावनाएँ प्रशान्त, निश्चल, स्नेहमय, प्रेम और पवित्रता से चित्रित न हों, तब तक रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती। चिकित्सक रोगी को शक्ति-संरक्षण हेतु मौन व्रत के पालन का भी आदेश देता है। ईसा ने एक जिज्ञासु को उपदेश दिया- "यदि तुम बुरी भावना रखते हो, तुमने अपने भाई को क्षमा नहीं किया और भगवान् को प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ, सर्वप्रथम अपने भाई को क्षमा करो, तत्पश्चात् पूजा में भगवान् की वेदी के निकट जाओ।" इसी प्रकार, प्राचीन भारत में वैद्य ने कहा- "यदि आपमें किसी के लिए भी घृणा, वैर और द्वेष के भाव हैं तो मैं आपकी चिकित्सा नहीं कर सकता, मैं आपको यह औषधि नहीं दे सकता; क्योंकि मेरी औषधि में आध्यात्मिक तत्त्व है, यह पावन एवं पुण्य है। सर्वप्रथम, आप अपने मन को सब असात्विक विचारों से मुक्त करो और फिर मेरे पास आओ, मैं आपकी चिकित्सा करूँगा।"
आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि रोग शरीर में नहीं, प्रत्युत मन में है। मानसिक रोग ही बाह्य शारीरिक रोग का कारण है। शारीरिक रोग को वे 'व्याधि' कहते हैं और मानसिक कारण जो शारीरिक रोग का मूल है, को 'अधिव्याधि' कहा। अधि का अर्थ है-मूल, प्रथम अथवा प्रारम्भिक। आभ्यन्तर संवेगात्मक अवस्था अधिव्याधि कहलाती है जिसका अभिप्राय है-प्रारम्भिक रोग! एक रोग से दूसरे रोग का जन्म होता है। एवंविध, अहितकर भाव, मन की असत्य वासनाएँ, अपनी प्राण-शक्ति, विराट् जीवन-शक्ति का दुरुपयोग तथा आक्रोश- ये सब शरीर की ऐसी अवस्था कर देते हैं जो रोग का कारण बन जाते हैं।
त्रिदोषों का आयुर्वेदिक सिद्धान्त
भारत के पुरातन ऋषियों ने शरीर की इन अवस्थाओं की पाश्चात्य ढंग से नहीं, प्रत्युत अत्यन्त अनूठे ढंग से व्याख्या की। उनका 'त्रिदोष' सिद्धान्त था। मन और प्राण की अशुद्धि के परिणाम स्वरूप अभिव्यक्त रुग्णावस्था का आयुर्वेदीय निदान (निर्णय) शरीर के दोषत्रय पर आधारित था। आयुर्वेदिक वैज्ञानिकों ने कहा- "मानसिक शुद्धि और प्राण-शक्ति की सूक्ष्मता में अव्यवस्था प्रत्येक मानव शरीर की सामान्यावस्था को चित्रित करने वाले दोषत्रय में सन्तुलन-विच्छेद का कारण हुई। यूरोप और इग्लैण्ड का मध्यकालीन चिकित्साविज्ञान 'दोषत्रय' के सिद्धान्त से पूर्णतः अपरिचित न था। मेरा विश्वास है कि यूरोप में उनके पास आयुर्वेद का समरूप ही कोई ग्रन्थ था और कदाचित् वह अरब और ग्रीस से आया था। तीन दोष हैं-वात, पित्त और कफ । स्वस्थ शरीर में ये दोष एक विशेष परिमाण में होते हैं और प्राण-शक्ति में दुरुपयोग, दूषण तथा अधिक व्यस्तथा के कारण विकार आ जाता है। इस प्रकार मन में वासनाओं तथा संवेगों के कारण विक्षेप आने पर 'दोषत्रय' (वात, पित्त, कफ) में असन्तुलन आ जाता है, तत्पश्चात् रोग के लक्षण अभिव्यक्त होने लगते हैं। इस असन्तुलन के कारण यदि कफ-विकार की अधिकता हो तो कफ सम्बन्धी सर्वरोग जैसे-श्वास रोग, फेफड़ों का रोग, खाँसी, जुकाम आदि संवृत होने लगते हैं। असन्तुलनवश वात-विकार की प्रधानता होने पर शरीर में पीड़ा, सन्धिवात (गठिया), वायु, कटिवेदना इत्यादि वात-व्याधियाँ घर करने लगती हैं।
वैद्यों द्वारा प्रदत्त औषधि से इस 'दोषत्रय' के असन्तुलन को ही सन्तुलित करना होता है; किन्तु वैद्य कहता है- "इस औषधि के द्वारा मैं सन्तुलन को पुनः युक्त करने का प्रयास कर सकता हूँ; किन्तु भीतर से आपको ही कार्य करना है ।'' अतः निश्चयेन प्रथम आवश्यकता है आत्म-संयम और द्वितीय-आक्रोशक भावों पर विजय । सब दुष्ट भावनाओं से मुक्त हो जाओ। कैसे? इस विषय में आयुर्वेदिक ऋषि सत्यतः सही भी थे। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की भाँति वे मनोविज्ञान से अनभिज्ञ थे, तथापि ज्ञातव्य ज्ञान का श्रेय उन्हें प्राप्त था। उन्होंने कहा- "यदि आप मन को संवेगों से मुक्त करके प्रशान्त करना चाहते हैं तो इसमें आध्यात्मिक तरंग उत्पन्न करो।" इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु वैद्य किसी विशेष धर्म-स्थल में परम देव के किसी विशेष रूप की विशेष उपासना-विधि बताते अथवा मन्त्र-विशेष के जप का आदेश देते।
उपासना आपके जीवन में एक शक्तिशाली साधन है; क्योंकि पुनः जब आपका मन ईश्वर में मग्न हो उठता है और आप अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ, उस स्रोत के साथ एक रूप करते हैं जिससे आपने सम्बन्ध विच्छेद कर दिया था और जो विच्छेद इस मनुष्य-जन्म, लौकिक अस्तित्व रूपी रोग का मूल कारण बना, तब उपासना मन को परिशुद्ध करती है। एक बार फिर जब आप उपासना में दिव्यस्वरूप परमात्मा के साथ एकस्वर होते हैं और मन्त्रों तथा दिव्य नाम का उच्चारण करना प्रारम्भ करते हैं, तब इस भौतिक शरीर में रोग के लक्षण के कारण स्वरूप मन सत्त्व को पवित्र, सूक्ष्म और स्थूल अवस्था प्रदान कर इसे परिशुद्ध किया जाता है। अतः बाह्यतः वैद्य और अन्तः रुग्ण व्यक्ति के सहयोग से शरीर को पुनः सुस्वस्थ स्थिति प्राप्त होती है।
जीवन के विज्ञान, पंचम वेद, आयुर्वेद का स्वास्थ्य के सिद्धान्त और विधि का यही सार है।
मनुष्य दिव्य स्वरूप है, आरोग्यता स्वाभाविक अवस्था है और शुद्धि तथा सूक्ष्मता आरोग्यता हेतु पूर्वापक्षित हैं-इस मूल धारणा पर आधारित आयुर्वेद के पास अत्यन्त रोचक स्पष्टीकरण है। जीवन के प्रति हिन्दू धारणा के अनुसार मनुष्य साधन-चतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) की प्राप्ति हेतु जीवन-यापन करता और कार्य करता है। धर्म आचार-नीति की पूर्ति है। अर्थ सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए धनार्जन है। पदार्थों के लिए सम्पत्ति को हिन्दू-धर्म में त्यागा नहीं गया। 'अर्थ' का अभिप्राय है-सुखी जीवन व्यतीत करने हेतु धन कमाना। 'काम' का अभिप्राय उन सब अनिवार्य इच्छाओं की पूर्ति है जो एक प्रतिष्ठित एवं पवित्र जीवन के लिए अनिवार्य तथा अपने और कुटुम्ब के कल्याण हेतु आवश्यक हैं। उन सभी अनिवार्य कामनाओं की पूर्ति 'काम' है जो जनगण के हित में बाधक न हो। अन्ततः मोक्ष, दिव्यस्वरूप परमात्मा में मुक्ति, शाश्वत स्वतन्त्रता है।
आयुर्वेद कहता है कि इस साधन-चतुष्टय की प्राप्ति हेतु हमारी आरोग्यता ही परम, सर्वश्रेष्ठ नींव है, आधार है। आरोग्यता के बिना इन चारों में से एक की पूर्ति भी असम्भव है। अतः शरीर को निरोग रखना अति महत्त्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। इसके लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए - (१) संयम और युक्तता द्वारा प्राण-शक्ति का संरक्षण, (२) सम्यक्-चिन्तन, भाव और श्रद्धा द्वारा मन की शुद्धि, (३) प्रशान्त मन से उचित समय पर उचित ढंग से लिया गया शुद्ध एवं युक्ताहार तथा भोजन के उपरान्त किंचिद् विश्राम द्वारा शरीर की देख-रेख करना।
एवंविध, स्वास्थ्य की उचित अवेक्षणा, प्राण-शक्ति की उचित संरक्षा और मन के सुविचारों द्वारा यदि आपका मन अच्छा है तो आप समृद्धिशाली जीवन की प्राप्ति हेतु भी क्या प्रयास करेंगे? समृद्धि का अच्छा स्तर कैसे प्राप्त हो? कदाचित् इसका अभिप्राय छल, कपट, लोभ और अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। उसका अभिप्राय है-आवश्यक सीमा के भीतर सुखी जीवन, जिसमें चित्त की शान्ति हो, जो चिन्ता, आवेग और अशान्ति से मुक्त हो, जिसमें आप अपना मन और विचार अपने साथी की सेवा में और भगवान् की अर्चना में लगा सकें, परोपकार कर सकें और स्वयं के लिए उपयोगी बनें। समृद्धि के नियम क्या हैं? मैं आपको समृद्ध बनने के रहस्य नहीं, वरंच समृद्धि के नियम बता रहा हूँ।
समृद्ध कैसे हों
समृद्धि का अर्थ निश्चयेन अपनी सीमा के भीतर रहना और जितना आप धनार्जन कर सकें, उससे न्यून व्यय करने में निहित है। ऋण कभी मत करो। सारांश में, यह अतीव बुद्धिमत्ता का कार्य है। समृद्ध कैसे हों? आप यदि एक सौ पचास डालर अर्जन करते हैं तो एक सौ उनचास डालर व्यय करें। इस प्रकार आपके पास एक डालर सदा शेष रहेगा। इस पर टिप्पणी करने की आज्ञा दें तो मैं कहूँगा- "अशांश व्यवस्था (किश्तों पर देना-लेना) में कभी मत उलझें।" आपके पास धन है, अस्तु । वस्तु खरीदें अन्यथा इसके बिना ही निर्वाह करें।
पुनरपि, समृद्धि के कुछ विशेष नियम हैं जो शाश्वत आध्यात्मिक सत्यों से भी उद्भुत हैं। यदि आप अभाव का विचार और अनुभव करने लगें तो आपको अभाव की ही अनुभूति होगी। यदि आप अधिक के भाव में प्रवृत्त हों, तो छाया की भाँति प्रचुरता आपका अनुसरण करेगी। इच्छा की भावना आने पर आप तत्काल निर्धनता को स्वीकार करते हैं। इच्छा निर्धनता है। इच्छा अपर्याप्ति का भाव है। इच्छा करने वाला व्यक्ति पूर्णतः भिक्षुक है। पूर्वजों का, समृद्ध रहने का रहस्य संवृद्धि के इस नियम के साथ दृढ़ता के साथ एवं सामान्य ज्ञान के वास करने में निहित था।
अज्ञानवश मनुष्य इच्छाओं का दास बन कर स्वयं को दीन समझने लगता है और निर्धनता ही उसका प्रारब्ध बन जाती है। समृद्धि के नियम को स्वच्छन्द गति देनी है। क्यों? समृद्धि का रहस्य आपके भीतर है। आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं क्योंकि आप स्वयं भगवान् के हैं जो सर्वस्व है। वह सर्वव्यापी है। सबका स्रोत वही है। उसी में सर्वस्व विद्यमान है और यदि आपको यह ज्ञान हो जाये कि आप उसी परमात्मा में व्याप्त हैं, तो आपके पास सब पदार्थ हैं और सब पदार्थों में आपकी सत्ता है। सदा उसमें लीन रहने के भाव का ज्ञान एवं इस तथ्य की धारणा समृद्धि की प्रधान कुंजिका है। तब समृद्धि आपका ऐसे अनुसरण करेगी जैसे श्वान अपने स्वामी का करता है।
अतः आप सकल सृष्टि के स्वामी हैं; क्योंकि आप उसके उत्तराधिकारी हैं जा सब पदार्थों का स्वामी है। आपको कोई अभाव नहीं है। समृद्धि और सर्व वैपुल्य तो आपकी निजी आत्मा है। आपकी वास्तविक प्रकृति पूर्ण स्वरूप है। विश्वास के साथ सदा से विद्यमान उस शाश्वत सत्ता को प्रमाणित करने के लिए जब आप प्रवृत्त होते हैं। तब समृद्धि आपके चरणों में आ जाती है।
अभाव अथवा दीन-भाव मन की एक तरंग है। आपके पास यदि पर्याप्त है और आप अनुभव करते हैं- "मेरे पास सर्वस्व है", तब आपको किसी पदार्थ का अभाव नहीं रहता; किन्तु पर्याप्त होने पर भी यदि आप सोचें कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास वस्तुतः कुछ नहीं है। एक करोड़पति जो सदा दस करोड़ अथवा बीस करोड़ बनाने की लालसा रखता है, वह यथार्थतः भिखारी है। एक बैलगाड़ी चलाने वाला या द्वार पाल तीन से चार रुपये प्रतिदिन प्राप्त करता है और कहता है- "मेरे लिए यह सुपर्याप्त है, मेरी जेब सदा भरी रहती है", सदा करोड़पति से महत्तर है। वह करोड़पति से अधिक धनवान् है; क्योंकि उसे अभाव अथवा अपर्याप्ति का क्लेश अनुभव नहीं होता और इच्छाओं का कार्पण्य भाव उसे नहीं सताता।
अतः पूर्णतः के भाव को दृढ़ करना, वैपुल्य को प्रमाणित करना और सदा प्राचुर्य की उसी नित्य अवस्था में वास करना, भगवान् को अपना मान कर सर्वस्व प्राप्ति की अनुभूति, समृद्धि का रहस्य है। मात्र यही विधि है। यही रहस्य है और जिस क्षण ही आप इनको निश्चित समझने लगेंगे, आप अपनी स्थिति में परिवर्तन का अनुभव करेंगे; क्योंकि आपकी दशा आपके अपने विचारों का ही परिणाम है। आपके जीवन का निर्माण करने वाला आत्यन्तिक विराट् तत्त्व आपके विचारों से विरचित है। वे इतने ही मर्मस्पर्शी एवं सारगर्भित हों जैसे ईंटें - जो समवेत हो कर एक बड़ा पर्वत बन जाती हैं। वे आपके सम्पूर्ण जीवन की रचना कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी अवस्था को जन्म दे सकते हैं। संकल्प द्वारा आपका निजी स्वास्थ्य सुधर सकता है। किसी वस्तु का आधार ले कर जैसे व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार संकल्प में निर्माण-शक्ति है और एक-एक कोष करके क्लिष्ट कोषों का निर्माण किया जाता है। संकल्प द्वारा आप अपनी विनष्ट क्षय-पूर्ति कर सकते हैं तथैव विकल्प, सम्पूर्ण विनाश कर व्यक्ति को रुग्ण बना देता है। संकल्प-शक्ति आपके हृदयंगत है। वह आत्मा से ही उद्भूत है; क्योंकि आत्मा ही आपके समीपतम है। आत्म-शक्ति सब संकल्प शक्तियों से परे है। आपकी यथार्थ प्रकृति का दृढ़ निश्चय उन सब अवस्थाओं का परिक्रमण करता है जो आपके लिए स्वाभाविक नहीं हैं, बाह्य हैं।
इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सन्तोष ही आपको विपुलता सुनिश्चित कर सकता है जो भी प्राप्त हो, पूर्ण का ही अनुभव करो। एक रुपये को एक लाख मानो और दस रुपये आपके पास हों तो उसमें दस करोड़ की अनुभूति करो। एक बार आप सन्तोष-धन प्राप्त कर लें तो आपको अन्य कोई पदार्थ प्रसन्न नहीं कर सकता।
सच्ची अनन्त प्रकृति एवं निज पूर्णता के भाव को ही सुदृढ़ करना चाहिए। यही समृद्धि का रहस्य है। सन्तुष्ट रहें और अपने मन से कहें- "किसी भी इच्छा को भीतर आने की आज्ञा नहीं है।" जिस क्षण इच्छा उत्पन्न हो, उसकी उपेक्षा करो और कहो- "इच्छा ! बाहर निकलो।" तदुपरान्त आप अनुभव करने लगेंगे कि अभीप्सित पदार्थ स्वयं ही आपके पास आता है। किसी विषय के पीछे भागने पर आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते; किन्तु उससे विमुख होते ही वह आपका अनुसरण करने लगता है। यह शाश्वत नियम है। स्वयं पर अनुभव करने वाले सत्यान्वेषियों ने इस नियम को प्रमाणित किया है। आप जितनी अधिक कामना करते हैं, उतनी अधिक आपके अभाव में वृद्धि होती है। यह सिद्धान्त आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए, हृदयंगम होना चाहिए।
समृद्धि का आध्यात्मिक सिद्धान्त
इससे ऊपर भी कुछ है! हिन्दू-धर्म के अनुसार इस ब्रह्माण्ड में जो-कुछ भी है, सर्व दिव्य तत्त्व है। प्रत्येक वस्तु भगवान् है। प्रत्येक शक्ति भगवान् है। प्रत्येक क्रिया भगवान् है। प्रत्येक जीव भगवान् है। प्रत्येक नाम और रूप भगवान् है। अनुभवगम्य प्रत्येक पदार्थ विविध अभिव्यक्तियों में ज्योतिरूप परमात्मा ही है और समृद्धि विश्व में दिव्य शक्ति के पोषक स्वरूप की साक्षात् अभिव्यक्ति है। इस वैश्विक प्रक्रिया में दिव्य शक्ति प्रथम संकल्प-शक्ति के रूप में आविर्भूत होती है जो प्राण-दान करती है और तत्पश्चात् तीन काल-भूत, वर्तमान और भविष्य में यह धारणा-शक्ति के रूप में क्रियाशील रहती है। संकल्प-शक्ति पोषण, संवर्धन और रक्षण करती है तथा इसकी देख-रेख करती है। युग के दूसरे किनारे पर भी आप भगवान् ही हैं। पुनः वही शक्ति सृष्टि को प्रलय द्वारा प्रसृष्ट गोचर पदार्थों को उनकी वास्तविक अदृश्य अवस्थाओं में विलीन कर देती है।
हमारे लिए परमात्मा का केन्द्रीय भाग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है जो विविध प्रकार से प्राणियों का रक्षण, धारण और पोषण करता है। दिव्य शक्ति अन्न के रूप में, ऋतुओं के रूप में, मेघ और वर्षा के रूप में विद्यमान है। भूगर्भ से प्राप्त वैपुल्य एवं समृद्ध शस्य के रूप में विद्यमान है। यह हमारे भीतर जठराग्नि के रूप में विद्यमान है जो भोजन को पचाती और हमारा पोषण करती है। सभी समृद्धि अवस्थाओं के रूप में भी यह विद्यमान है।
एवंविध, अन्न ब्रह्म है। बाह्यतः अन्न ब्रह्म का साक्षात् स्वरूप है। आपके अन्तःकरण में प्राण-शक्ति ब्रह्म है। जीवन पालन करने वाले सब पदार्थ ब्रह्म की अभिव्यक्तियाँ हैं। महती जीवन-शक्ति ब्रह्म है। आपके अन्तस्तम अस्तित्व में चैतन्य से प्रभावित प्रज्ञा-ज्योति ब्रह्म है।
अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, क्रोध अथवा क्षोभ की स्थिति में भोजन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं! भोजन के समय एक हिन्दू सर्वप्रथम मुट्ठी-भर चावल ले कर विनयपूर्वक मस्तिष्क तक ले जाता है, नमस्कार करता है और फिर भक्ष्यार्थ कौर मुख में डालता है। भोजन को प्रणाम करके ही वह इसे ग्रहण करता है।
अतः भोजन अवज्ञापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक अथवा गुण-दोष का विवेचन करके नहीं करना चाहिए। “यह कैसा भोजन तुमने तश्तरी में रख दिया है?" भोजन के समय इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। आराधनापूर्ण ढंग से भोजन ग्रहण करो। भोजन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भोजन व्यर्थ छोड़ना भी एक प्रकार से अन्न का तिरस्कार है, दुरुपयोग है। भोजन को व्यर्थ करने वाला व्यक्ति समृद्ध नहीं होगा।
अन्न शरीर में शक्ति के रूप में समन्वित होता है। अतः जीव की प्राण-शक्ति को भी ब्रह्म की उपाधि दी जाती है। यह दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह सम्मान और आदर के योग्य है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और इसका विनाश नहीं करना चाहिए।
ऐसा व्यक्ति समृद्धिशाली होता है। आत्यन्तिक विश्लेषण में, आपके सब विचार और भावों की पवित्रता अनिवार्य है। समृद्धि सत्य में है, पवित्रता में है। समृद्धि दया और करुणा में तथा अच्छे भाव में है। यदि आप सर्वदा परोपकार, पर-समृद्धि, पर-कल्याण की भावना रखते हैं तो आप अनायास ही समृद्धि प्राप्त करते हैं। समृद्धि का अभिप्राय करोड़ों की सम्पत्ति से ही नहीं, वरंच अभाव की अनुभूति न होने से है। आप कभी दुःखी न होंगे। भगवान् आपका ध्यान रखेगा और आपके सब अभावों को दूर करेगा। प्रत्येक क्षण, आपकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति भगवान् करेंगे।
हमें बोध करना है कि समस्त मानव जीवन परब्रह्म परमेश्वर द्वारा संचालित हो रहा है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का वह अन्तर्निदेशक है। समस्त सृष्टि का वह अन्तः संचालक है और आपके जीवन का पथप्रदर्शन भी वही कर रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षण में यदि आप समृद्धि के नियमों का पालन करेंगे, अन्न, प्राण-शक्ति, सम्पत्ति, स्वसद्गुण एवं विचार और बुद्धि आदि विविध रूपों में ब्रह्म की विभिन्न अभिव्यक्तियों का सम्मान करेंगे तथा उनका सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं करेंगे, विनीत भाव से उनका सम्मान करेंगे तो समृद्धि निश्चित है। तब समृद्धि आपके चरणों में वास करेगी। आपका गृह परिपूर्ण कर देगी। वह वास-स्थान सदा तेज, हर्ष, दान, सद्भाव से भरा रहेगा जहाँ समक्ष रखे भोजन का सम्मान होगा और विनीत भाव रहेगा।
गृह-समृद्धि हेतु कतिपय अमोघ सूत्र
हिन्दू होने के नाते मैं आपको चार-पाँच सूत्र बताना चाहता हूँ। जहाँ वृद्ध जनों का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि का साम्राज्य होता है और जहाँ माता-पिता, पितामह, पितामही, चाचा, चाची से तिरस्कारपूर्ण कठोर व्यवहार किया जाता है, उनका स्वल्प आदर किया जाता है, वहाँ समृद्धि नहीं होती।
सामान्य जनों को यह ज्ञान नहीं होता। अतः जब विपत्ति आती है, वे दुःखी होते हैं, जब समृद्धि का अभाव होता है तो यह ज्ञान नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ। इन नियमों की सर्वथा उपेक्षा करने पर व्यक्ति स्वयं इन कष्टप्रद अवस्थाओं का आह्वान करता है। तत्पश्चात् आप दुःखद परिस्थिति के परिणाम खोजने का यत्न करते हैं-पुस्तिका में देख कर अथवा आय-व्यय का मूल्यांकन लगा कर, कदाचित् आप आर्थिक अवस्था को दोषी ठहराते हैं। किन्तु नहीं-आध्यात्मिक सिद्धान्तों के उल्लंघन द्वारा आप इन परिस्थितियों को जन्म देते हैं। जहाँ बड़ों का आदर-सम्मान होगा, उनके प्रति श्रद्धा-भाव होगा, वहाँ उस परिवार में, उस घर में समृद्धि का वास होगा। वृद्ध जनों का सम्मान करने वाले व्यक्ति का जीवन सदा समृद्धि का आस्थान होगा।
द्वितीयतः, जहाँ गृह-भार्या के साथ विनीत व्यवहार किया जायेगा, उनका स्थान प्रथम होगा, जिसके वे योग्य हैं, वहाँ समृद्धि होगी। स्तर क्या है, मानवता कहाँ हैं यदि वह नारी के लिए नहीं हैं तो? वहाँ 'माँ' ही सृष्टि का मूल स्रोत है और जहाँ माताओं व गृहणियों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया जाता है, उस गृह में समृद्धि होती है। जिस घर में नारी का अपमान होता है, उसके साथ निर्दय, कठोर व्यवहार किया जाता है, वहाँ समृद्धि नहीं आ सकती। जिस घर में पत्नी और माँ को रुलाया जाता है, जहाँ वे अश्रुपात करती हैं, वहाँ समृद्धि नहीं हो सकती। जिस गृह में नारी अश्रुपात करती है, वहाँ समृद्धि मानो पंख लगा कर उड़ जाती है।
तृतीयतः नारी-जाति के लिए भी नम्रता समृद्धि का लोहकान्त (चुम्बक) है। लज्जा नारी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। नारी का आभूषण, उसका सौन्दर्य, आभूषण अथवा पोशाक नहीं हैं, जिन्हें वह धारण करती है। नहीं, वह सौन्दर्य नहीं है। तो फिर शरीर का सौन्दर्य क्या है? जिस क्षण आत्मा इस शरीर का त्याग करती है, उसी क्षण यह शरीर वृथा हो जाता है। अतः नारी का वास्तविक सौन्दर्य उसका विनम्र स्वभाव तथा शालीनता में निहित है। पतिव्रता और लज्जाशील नारी पूज्य है। जिस परिवार में गृहणियों का श्रृंगार पातिव्रत्य, लज्जा और शालीनता हैं, वहाँ समृद्धि दासी बन कर रहती है।
आधुनिक उच्च समाजों में कभी-कभी नारी को परदे से बाहर देखना शोचनीय प्रतीत होता है। वे निज स्त्रीत्व गुण को विलुप्त कर रही हैं। अन्ततः कोमलता, लावण्य, सहृदयता, क्षमाशीलता और सहनशीलता आदि स्त्री के गुण ही उसे स्त्री की संज्ञा देते हैं। इन गुणों से युक्त स्त्री देवी तुल्य है। जहाँ स्त्री इन गुणों से हीन हो, वाग्प्टु हो, प्रखर हो, वैर-द्वैष-भाव से युक्त हो, वहाँ समृद्धि असम्भव है। जिस स्थान पर स्त्री हर क्षेत्र में पुरुष तुल्य होने की आकांक्षा रखे, वहाँ समृद्धि नहीं हो सकती। नहीं! उसे किंचित् विशेष समानता का अधिकार है; परन्तु प्रत्येक क्षेत्र में नहीं। पुरुष के साथ एक होने की लालसा में अपनी लज्जा, नम्रता, पातिव्रत्य-भाव का त्याग करना स्त्री के लिए प्रभु के अमोघ वरदान को खो देने के समान है।
एक वैदिक उक्ति है- "जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है (यत्र नार्याः पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः) ।" किन्तु जहाँ अपने ही कठोर आचार से नारी अपनी पूजा का अधिकार खो देती है, वहाँ समृद्धि नहीं आ सकती।
अन्ततः जहाँ भगवान् की आराधना होती है, वहाँ सम्पूर्ण गृहस्थ उच्चतम ऐश्वर्य से आनन्दित रहता है। सर्व सुख, सर्व आनन्द, सर्व समृद्धि उस सदन में पदार्पण करती है जहाँ नियम से भगवान् की पूजा होती है।
प्रातः उठ कर अपने स्वास्थ्य, शरीर, शुद्ध मन, स्वयं तथा अन्य जनों के कल्याण हेतु परोपकारी जीवन व्यतीत करने के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। सायंकाल पुनः सुदिवस के प्रसाद हेतु, निर्मल जलवायु, शीतल वायु, अच्छा स्वास्थ्य एवं शक्ति, सेवा के अवसर एवं परोपकार करने का अवसर प्रदान करने के लिए उस प्रभु का धन्यवाद करो। प्रतिदिन यदि प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने घर में प्रभु की आराधना करोगे, तो समृद्धि सुनिश्चित है।
जहाँ भगवान् की पूजा होती है वहाँ प्रभु साक्षात् रूप से विद्यमान रहते हैं और जहाँ देव की सुस्पष्ट विद्यमानता हो, वहाँ तो ऐश्वर्य और समृद्धि का कहना ही क्या है? वह घर सबके श्रेय, आनन्द से अभिव्याप्त एवं परिपूर्ण हो जायेगा। जिस प्रकार प्रकाश के साथ तेज और कान्ति निश्चित है, उसी प्रकार से जहाँ भगवान् है, वहाँ सर्व मंगल, आनन्द और समृद्धि सुनिश्चित है। अतएव यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो उपासक बनें। केवल मन्दिर को ही अपनी प्रार्थना और पूजा का स्थान न बनायें। प्रत्येक घर भगवद्-पूजा का केन्द्र ब जाये। प्रत्येक घर भगवद्-प्रार्थना का केन्द्र बन जाये। प्रत्येक घर भगवद्-धाम बन जाये। स्त्रियाँ नम्रता, पातिव्रत्य, पवित्रता, गम्भीरता की प्रतिमूर्ति बन जायें। परिवार के शिशु एवं पुरुष स्त्रियों को यथोचित सम्मान प्रदान करें और उनसे दया, सद्भावना, सदाचार का व्यवहार करें जिसके वे योग्य हैं। शिशु अपने बड़ों को सम्मान प्रदान करें। यदि इन नियमों का पूर्णतया पालन किया जाये, तो समृद्धि एक स्वयंसिद्ध अवस्था बन जायेगी। ऐसे घर में तब न कोई इच्छा रहेगी, न समस्या और न ही कोई अभाव होगा।
पूर्वजों का आत्यन्तिक ज्ञान यही है। वे कहते हैं-"मनुष्य का स्वभाव ही समृद्धि का निर्माता है।" बाह्य तत्त्व तो गौण है, प्रमुख नहीं।
८. शक्ति देवी के रूप में भगवद्-आराधना
ज्योतिर्मय अमर आत्मन्! दिव्य सत्ता को प्रणाम ! भगवद्-कृपा से सम्पूर्ण विश्व में शान्ति हो और समस्त मानवता पर सुख और कल्याण की वृष्टि हो!
पाश्चात्य देशों में हिन्दू-धर्म के नाम से प्रसिद्ध हमारा सनातन-धर्म, जो जीवन की प्राचीन वैदिक पद्धति है, जीवन के लक्ष्य के रूप में हमें भगवद्-साक्षात्कार द्वारा, पार्थिव बन्धन और मृत्यु से शाश्वत मुक्ति को जीवन का चरम लक्ष्य बताता है। आध्यात्मिक साक्षात्कार और शाश्वत आनन्द की यह अवस्था मोक्ष अथवा कैवल्य की उपाधि से आख्यात है। दुःखानुभवों से निवृत्ति और परम आनन्द से संलक्षित यह परम सुख और शाश्वत सन्तोष की अवस्था है। आप जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं।
इस परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनुकूल एवं सुखावह जीवन के आदर्श और आकांक्षित व्यवस्था को भी लक्षित करते हुए सनानत-धर्म मोक्ष के अतिरिक्त तीन अन्य उद्देश्यों का वर्णन करता है जो क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रथम-धर्म अर्थात् सच्चरित्रता । द्वितीय-अर्थ अर्थात् जीवन-निर्वाह के लिए सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संघर्ष, जिसमें धर्म के नियमों का उल्लंघन न हो। तृतीय-अपने विविध कर्तव्यों का पालन करते समय उत्पन्न अनिवार्य व्यक्तिगत निष्काम इच्छाओं की पूर्ति! यहाँ भी इच्छाएँ धर्मादेशों के प्रतिकूल न हों। अतः यह स्मरणीय है कि मोक्ष-प्राप्ति की उक्त प्रक्रिया में सर्वत्र धर्म का ही साम्राज्य है। एक सच्चे सनातनधर्मी को प्रत्येक दशा में, प्रत्येक अवस्था में धर्मनिष्ठ होना चाहिए। एक सच्चा सनातनी हिन्दू वह है जो एक क्षण के लिए भी स्व-जीवन के परम दिव्य लक्ष्य को विस्मृत नहीं करता और सदा इसका स्मरण करते हुए अपना समस्त जीवन धर्म अथवा सदाचार पर आधारित करता है।
बहुधा, एक सच्चे सनातनधर्मी हिन्दू के समक्ष भगवद्-साक्षात्कार द्वारा अन्तिम लक्ष्य मोक्ष ही मुख्य उद्देश्य होने के कारण इस प्राचीन धर्म में इसकी प्राप्ति हेतु भी स्पष्ट रूप से साधन अथवा विधियाँ वर्णित हैं। अनेक साधन और युक्तियाँ प्रस्तुत की गयी हैं; किन्तु असंख्य और सर्वथा पृथक् होते हुए भी उन्हें एक शब्द 'आराधना' के अन्तर्गत समाहित किया जा सकता है। भगवद्-अनुकम्पा की अभिव्यक्ति कराने वाली 'आराधना' द्वारा ईश्वर-प्राप्ति सुलभ है। भगवान् के समीप उपासना ही 'आराधना' है। वन्य जनों की अनगढ़ पत्थर अथवा पशु-पूजा से ले कर सर्वोच्च समाधि की अवस्था पर्यन्त, जिसमें परम चैतन्यावस्था में साधक मन और इन्द्रियों से ऊपर उठ कर केवल भगवान् की ही अभ्यर्थना करता है और इसके अन्तर्गत आराधना के सभी रूप और प्रकार अन्तर्भूत हो जाते हैं। आराधना के भीतर ही आराधक और आराध्य का द्वैत निहित है। इष्टदेव की धारणा के साथ इस आराधना-पद्धति का साक्षात् सम्बन्ध है। विशेषतः इसी सन्दर्भ में हम मातृ शक्ति की आराधना के उद्भव के दर्शन करते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में, जगदम्बा के रूप में ईश्वर-आराधना का दर्शन करते हैं।
देवी-पूजन का उद्भव
जगदम्बा के रूप में भगवान् की मनुष्य के लिए विशेष महत्ता है। इसके अनेक कारण हैं। प्रथमतः, शिशु रूप में मानव-प्राणी माँ से सर्वप्रथम अवगत होता है। माँ ही सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली सर्वोपरि शक्ति है और एक अवस्था-विशेष में सर्वस्व वही है। द्वितीयतः, इस धरती पर माँ का सम्बन्ध सब मनुष्य-सम्बन्धों में मधुरतम और प्रेमाप्लावित है। तृतीयतः, पुरुष का पौरुष सदा एक परुषत्व और अनुशासन से बँधा हुआ होता है, जब कि मातृस्वरूप अनवरत ममता, दया, परिपोषक रक्षण, सहनशीलता और क्षमा से भी आपूरित होता है। अतः भ्रान्त मनुष्य यदि परम पिता परमात्मा की अपेक्षा जगद्-जननी की ओर आकर्षित होता है तो कोई आश्चर्य नहीं। सुख, शान्ति और क्षमा का अभ्याकांक्षी मानव पिता की ओर नहीं, माँ की ओर उन्मुख होता है। कठोर अनुशासन में पिता ही रख सकता है; किन्तु माता से उत्कण्ठा, क्षमा और स्नेह आकांक्षित है। एवंविध, युगों से मनुष्य ने परम दिव्य सत्ता की जगज्जननी के रूप में आराधना करने की समय-बद्ध परम्परा स्थापित की है।
शक्ति की इस आराधना में मनुष्य स्वयं को स्वभावतः ही माँ का एक शिशु अनुभव करता है। यही भाव सार-रूप में इस पहुँच की विधि है। जिस प्रकार एक शिशु माँ की आदर्श देख-रेख में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ माँ के अधिक समीप जाता है उसी प्रकार आराधक आत्मसमर्पण-भाव और श्रद्धा से प्रेमाई हो कर 'माँ' की स्तुति करता है। इस आराधना से आराधक के व्यक्तित्व में गहन रूपान्तरण होता है। कठोर 'अहं' शिशुजन्य आर्जवता में रूपान्तरित हो जाता है। कुटिलता सरलता में परिणत हो जाती है। स्व-प्रतिपादित दर्प, मौन शान्ति का रूप धारण कर लेता है। भय और सम्भ्रान्ति अभय और श्रद्धा में परिणत होती है। इस प्रकार देवी माँ की आराधना होती है।
माँ का अर्थ है-प्रेम। माँ का अर्थ है दया। माँ का अर्थ है-संरक्षण और सहज देख-रेख । मन से भली-भाँति यह दृढ़ धारणा करनी चाहिए कि माँ की आराधना का एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक स्तर हो और इस प्रकार की सब आराधनाओं के अन्तिम लक्ष्य भगवद्-साक्षात्कार की ओर अग्रसर करने में माँ प्रभावपूर्ण है। आराधना की प्रक्रिया का लक्ष्य आपकी चेतना को क्रमशः देवत्व में परिणत करना है। दिव्यानुभूति हेतु आपको दिव्य बनना होगा। माँ के प्रेम और कृपा का आह्वान करने के लिए आपको प्रेम का प्रकाश-पुंज बनना होगा। दिव्यता में आरोहण करने के लिए तमस् से रजस् और रजस् से सत्त्व की ओर तथा सतत्त्व से शुद्ध सत्त्व की ओर उत्थान करना होगा, जहाँ से त्रिगुणातीत हो कर व्यक्ति दिव्य स्वरूप बन जाता है। अतः देवी माँ की सच्ची और विधिपूर्वक पूजा सर्वोच्च सात्त्विक गुण की उच्च आध्यात्मिक विधि है। देवी का शुद्ध भावुक (अकर्ता) स्वरूप यदि कठोर और दूरस्थ है तो उसका निजी स्वरूप कोमल, उदरस्थ, प्रगाढ़ और पूर्णतया समुपगम्य है। मातृदेवी प्रेम-स्वरूप है जो भक्त का हृदयालिंगन करने के लिए भुजा फैलाये प्रतीक्षा करती है।
देवी-पूजन के विविध स्वरूप
आधुनिक हिन्दू-समाज में प्रचलित देव्याराधना के तीन-चार विविध रूप हैं। शक्ति के कतिपय विशेष विभाग (के भक्त) शाक्त तन्त्रों में विहित विधि के अनुसार भक्ति-भाव से देवी की आराधना करते हैं। आराधना का यह अत्यन्त कलात्मक स्वरूप है जिसमें एक विशेष क्रमागत ऋत का पालन किया जाता है और शक्ति-परम्परा के अनुसार इसमें प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षा देनी पड़ती है। शाक्तों के कतिपय अन्य विभाग हैं, अशाक्त भी हैं जो सहज विधियों द्वारा पवित्र भक्ति-भाव से पूजा में संलग्न होते हैं। तान्त्रिक पूजा विधि की अपेक्षा यह कम कलात्मक है। इसमें भक्त देवी को प्रेम के रूप में आवाहन करने में प्रवृत्त होते हैं।
पुनः, 'नवरात्र पूजा' के नौ दिवस पर्यन्त सम्पूर्ण भारत में सब प्रकार के लोगों द्वारा देवी की आराधना की जाती है। देश-व्याप्त इस वार्षिक पूजा में माँ का कल्याणकारी, आनन्दमयी और समृद्धिदायिनी के रूप में आह्वान किया जाता है।
देवी-पूजन के एक अन्य स्वरूप का विषय यहाँ देना अयुक्त न होगा। वस्तुतः यह आराधना का अशुद्ध और अधम स्वरूप है जो त्याज्य है। यह है—अन्ध-विश्वास और भय से युक्त देव्याराधना ! इसके अन्तर्गत माँ को क्रोध और हिंसा से परिपूर्ण रौद्र रूप देवी माना गया है। इसमें वह प्रेम की अपेक्षा दण्ड देने के भाव से आपूरित होती है। वस्तुतः यह देवी-पूजन नहीं है। यह मातृत्व-भाव की अवहेलना है। यह आराधना का तामसिक स्वरूप है जो आराधना में पाप, भय, अत्याचार के तामसिक गुणों को उत्तेजित करता है। अपने रौद्र देव को शान्त करने के लिए आराधक अन्य प्राणियों की हिंसा-रूपी कुत्सित कर्म करने का आश्रय लेता है। वह प्राण लेता है जिसका वह पुरावर्तन नहीं कर सकता। इसलिए उसे प्राण-हरण का कोई अधिकार नहीं है। अज्ञानान्ध आराधक यह विचार नहीं कर सकता कि मातृ-देवी केवल मनुष्य की ही नहीं, वरन् समस्त सृष्टि की माँ है। मछली, खग, पशु, कीट-सब दिव्य माँ की सन्तति हैं। सर्व जीव पावन हैं। प्राण-हरण पाप है। नीति के अनुसार यदि मनुष्य की हिंसा अपराध है तो मूक पशुओं की हिंसा धर्म के विरुद्ध है, अपराध है। देवी के नाम पर उनकी हिंसा स्वयं भगवान् की अवज्ञा करना है। ऐसा अपराध दिव्य अनुकम्पा की वृष्टि नहीं कर सकता। यह विपत्ति के रूप में अप्रत्यक्ष परिणाम ही प्रदान करेगा। आराधना में प्रेम और दया के सार्वभौम धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। किसी नाम की होड़ में हिंसा का अपराध क्षमा नहीं हो सकता। अज्ञान और अन्ध-विश्वास तो इसका अनुमोदन कर सकते हैं; पर सनातन धर्म इसकी अनुमति नहीं देता।
एवंविध, शक्ति-आराधना का अन्तिम रूप वास्तव में आराधना के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता; क्योंकि यह आराधक को भगवान् से दूरातिदूर ले जा कर अन्ततः नरक में उसका प्रक्षेप करता है। ऐसी आराधना का स्व-स्वरूप ही उपेक्षणीय है। यह तत्काल त्याज्य है। जितना शीघ्र आप इसका त्याग करेंगे, उतना शीघ्र ही आपका कल्याण होगा।
मातृ-शक्ति के एक रूप-विशेष से सम्बद्ध एक अतीव महत्त्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। अनेक अवसरों पर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महापार्वती अथवा दुर्गा आदि विविध स्वरूपों में उसकी आराधना की जाती है। दुर्गा के रूप में मातृदेवी का आवाहना अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और भ्रम आदि दुर्गुणों का विनाश करने वाली शकि का आवाहन है। ये अन्धकारयुक्त अधम गुण आपके भीतर पशु का निर्माण करते हैं। मनुष्य के भीतर मानो यह अपवित्र पशुरूप हैं। आराधक से अहंकार, लोभ, मोह अनृत और घृणा से निर्मित निम्न प्रकृति का यज्ञ में आहुति दे देना आकांक्षित है। यह सच्चा अनुष्ठान है जो आराधक को जागृत करके उसे ईश्वर के समीप ले जाता है।
सहानुभूति, शान्ति, दया, क्षमा, सत्य और सरलता के पुष्पों से देवी की आराधना करो। प्रेममयी माँ के रूप में उसका अभिगमन करो। मोक्ष-रूपी सर्वोच्च आनन्द प्राप्त करने के लिए उसके पास जाओ। तब वह सर्वशक्तिमान् परमात्मा के स्वरूप से भिन्न न होगी और वह आपको कैवल्य मोक्ष का वरदान देगी। सनातन-धर्म की दिव्य सन्तान! इस सर्वोच्च उपहार के लिए उसका उपगमन करो, भौतिक तुच्छ पदार्थों की प्राप्ति हेतु नहीं। मातृदेवी की आराधना की वास्तविक महिमा यही है कि सृष्टि के रचयिता, विधाता, भगवान् की अपेक्षा माँ शीघ्रतर वर प्रदान करती है। जहाँ भगवान् से न्याय अपेक्षित है, वहाँ मातृ-शक्ति क्षमा और रक्षा की प्रतीक है। इसी कारण से जगदम्बा के भक्त अपनी विधि की प्रशंसा करते हैं।
९. गृह में योग
अब हम इस महत्त्वपूर्ण विषय को लेते हैं कि सांसारिक क्रिया-कलापों में व्यस्त होते हुए भी मनुष्य किस प्रकार पृथ्वी पर अपने जीवन के परम उद्देश्य अर्थात् आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। इहलौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों आपके जीवन के अंश हैं; क्योंकि ऐतिहासिक जीवन आपका बाह्य जीवन है, जब कि पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक जीवन की स्थिति आपके अन्तःकरण में है। पुनरपि आपके आध्यात्मिक जीवन की झलक बाह्यतः भी अवश्य दृष्टिगोचर होती है। आप जहाँ भी हों, आपकी आध्यात्मिकता साथ होगी। आप यदि गृहस्थी में हैं और सांसारिक कर्मक्षेत्र में परिश्रमी तथा व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपका आध्यात्मिक जीवन भी वही होगा। परिस्थितियों में अथवा अन्तरंग में बाह्य स्पष्ट परिवर्तन ला कर इस आन्तरिक जीवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। आप बैंकुवर की अपेक्षा रोम में श्रेष्ठतर आध्यात्मिक जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। भूमि की अपेक्षा पर्वत-शिखर पर रह कर आप अधिक आध्यात्मिक मानव नहीं बन सकते। भूगोल इसे परिणत नहीं कर सकता। मात्र बाह्य रूप के परिवर्तन वस्तुतः और सत्यतः आपके आध्यात्मिक जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते; क्योंकि यह आत्मा का जीवन है और आप जहाँ भी रहें अन्तरात्मा, भगवान् को देख सकते हैं। पवित्रतम तीर्थस्थानों में तो भगवान् ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं; किन्तु आपकी आत्मा यदि उसमें नहीं है और आप उसका उद्धार नहीं करते तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कदापि वास नहीं कर रहे।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक जीवन-गाथा
महर्षियों ने इस सत्य को साधकों के समक्ष उन्मीलित करने का विविध प्रकार से प्रयत्न किया है। मुझे एक घटना, एक अत्यन्त रोचक कथा स्मरण हो आयी है जो अधिक पुरानी नहीं है। यह विख्यात स्वामी विवेकानन्द के अध्यात्म-गुरु श्री रामकृष्ण के जीवन की है। अपने प्रारम्भिक जीवन में श्री रामकृष्ण उस समय की भारत की राजधानी कोलकाता के हिन्दू-मन्दिर में पुरोहित थे। यह मन्दिर एक तथाकथित छोटी रानी के द्वारा बनाया गया था जो उस समय के राष्ट्रीय अधिपति की अर्धांगिनी थी और विपुल धन-सम्पन्न थी। उसने प्रचुर सम्पत्ति व्यय कर मन्दिर का निर्माण करवाया और उसे सम्पन्न भूमि से सुशोभित किया। अपार धन-सम्पत्ति और वैभव से युक्त होने पर भी वह अत्यन्त भक्तिमती थी। अपनी सम्पत्ति की देख-रेख से सम्बद्ध होने पर भी उसका जीवन आध्यात्मिक था। प्रायः वह पूजा के समय मन्दिर जाती और देवतागार में बैठती। उस समय श्री रामकृष्ण परमहंस एक युवक पुरोहित थे। कदाचित् उनकी आयु चौबीस-पच्चीस वर्ष की होगी। इस अवसर पर भगवती गंगा-स्नान द्वारा पवित्र हो कर प्रभु की शरण में ध्यानमग्न बैठी होती। जब देवता की, स्तोत्रों द्वारा स्तुति और महिमा-गान करने का विशेष समय हुआ तो पूर्व इसके कि श्री रामकृष्ण गान प्रारम्भ करते, इस आर्या ने कहा- "क्या आप अमुक गान गायेंगे?" और उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दे कर भगवती की स्तुति प्रारम्भ की। गाते हुए अकस्मात् ही वे रुकते-से देखे गये। वे उस आर्या की ओर मुड़े और उसके पृष्ठभाग पर एक गूँजती हुई चपत लगायी और कहा- "क्या! यहाँ भी?" बस, इतना ही दृश्य देखा गया और इसके पश्चात् उन्होंने पुनः गान प्रारम्भ कर दिया। इस आर्या के साथ कुछ हथियार-युक्त रक्षक थे जो मन्दिर तक उसका अनुसरण करते हुए आये थे, सब स्तम्भित रह गये। कुछ भय से कम्पित होने लगे और कुछ विचार करने लगे-"अब इस व्यक्ति का अन्त समीप आ गया है। कदाचित् वह उसको बन्दी बनाने की शीघ्र ही आज्ञा दें", किन्तु यह देख कर वे आश्चर्यचकित हो गये कि वह आर्या अकस्मात् नम्न हो गयी और शान्ति से एकाग्र चित्त हो कर गीत श्रवण करने लगी-मानो पिता ने अपनी पुत्री की ताड़ना की हो। गान की समाप्ति पर आरती का क्रम हुआ और आरती समाप्त होने पर वह बाहर ऐसे आयी मानो कुछ हुआ ही नहीं। संरक्षक और कार्यकर्ता प्रतीक्षा में थे और आश्चर्यान्वित हो रहे थे-"न जाने क्या होने वाला है?" और प्रमुख कार्यकर्ता ने उससे प्रश्न किया- "कोई आज्ञा है? जो घटित हुआ, मैंने सब देखा; किन्तु देवतागार में पग न रख सका और कुछ भी करने में असमर्थ रहा।" रानी ने सहज भाव से कहा-"नहीं, कोई आज्ञा नहीं!" कुछ समयोपरान्त उसके जामाता ने यह बात सुनी जो उसकी ओर से मन्दिर का सारा प्रबन्ध करते थे। उसने रानी से इस सम्बन्ध में पूछा, तो रानी ने उत्तर दिया- "रामकृष्ण सर्वथा उचित था। मैंने उसे भगवती की स्तुति करने को कहा था; क्योंकि माँ ही वहाँ पर स्थापित थीं। जब वह गा रहा था, तो मैं उच्च न्यायालय में कल आने वाले सम्पत्ति के सम्बन्ध में व्यवहार पद का चिन्तन कर रही थी और उसके प्रति चिन्तित थी। मुझे और कोई चिन्ता न थी। मैं उसके गीत अथवा मातृदेवी का चिन्तन नहीं कर रही थी। ला-सूट मेरे मन को घेरे हुए था और मुझे दण्ड मिलना चाहिए था सो उसने किया। वस्तुतः उसने तो कुछ नहीं किया, माँ ने किया।" अतः वह आर्या मन्दिर में उपस्थित होते हुए भी मन्दिर में नहीं, प्रत्युत न्यायालय में थी। आपका अन्तःकरण ही इस बात का निर्णायक है कि आप आध्यात्मिक जीवन यापन कर रहे हैं अथवा भौतिक जीवन। जिस स्थान पर आसीन हैं, वह इसका निर्णायक नहीं। वही अन्ततः और बाह्यतः यौगिक जीवन व्यतीत करने के रहस्य का उन्मीलन करता है।
आप अपना जीवन आध्यात्मिक बनायें तो प्रत्येक वस्तु यौगिक बन जाये। पावन ग्रन्थ भगवद्गीता में जीवन के आध्यात्मीकरण की विधि अत्यन्त सुन्दर रूप से वर्णित है। दिव्य सत्ता के साथ ऐक्य भाव ही योग है और उसके प्रति महान् भक्ति-भाव से, परमात्मा के साथ सच्चे प्रेम से अनवरत आन्तरिक योग में व्यतीत करने पर आप कुछ भी करें, आप कुछ भी हों और किसी भी ढंग से रह रहे हों, आप यौगिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं; क्योंकि आप भगवान् के साथ रह रहे हैं और भीतर से आप भगवान् से अभिन्न हैं।
परमात्मा के साथ अभिन्नता का ऐसा जीवन, प्रेम और भक्ति में सदा उसके साथ योग करने के लिए सतत प्रयत्नशील जीवन और यह जागृति कि सम्पूर्ण जीवन का उद्देश्य पूर्णतया इस योग की पूर्ति है—यही दिव्य जीवन है। यही यौगिक जीवन है। यदि आप चेतन रूप से तत्त्वतः उसके समीप पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं तो आप यौगिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके बाह्य जीवन का कुछ भी रूप क्यों न हो।
यौगिक जीवन व्यतीत करने के लिए यह भावना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए यह भाव अत्यन्त अनिवार्य तत्त्व है। इसके प्रकाश में हम उन तत्त्वों की खोज कर सकते हैं जिन्हें अपने दैनिक गृहस्थ जीवन में सम्मिलित किया जाये, तो वे हमारे जीवन के अन्तस्तल में आत्म-साक्षात्कार करने में सहायक हो सकते हैं।
मानव-जीवन के चार प्रमुख स्वरूप
निश्चयेन हम स्वीकार करते हैं कि जीवन में हमें सर्वप्रथम अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहना चाहिए। सदा चेतन रहो कि आप क्यों जी रहे हैं। जीवन में किस उद्देश्य की पूर्ति करनी है, इसके प्रति जागरूक रहो। यही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृत्य है। यह ज्ञात कर लो कि जीवन का समाहित अभिप्राय परम लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु प्रत्येक क्षण का समुचित उपयोग करना है।
जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य के प्रति आप पूर्वतः ही सजग हैं कि परमात्मा में ही सच्ची शान्ति और सुख की अवस्थिति है, परमात्मा में ही इस मर्त्य अस्तित्व की अशुद्धियों का निराकरण हो सकता है, परमात्मा सर्वशोकातीत है और कैवल्य की अवस्था, अमरत्व, मुक्ति और अभय परमात्मा में ही प्राप्त हो सकते हैं। यह जानते हुए आपमें पूर्वशः ही आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की एक उत्कण्ठा और आकांक्षा जागृत कर दी गयी है जिससे परम लक्ष्य की प्राप्ति यहीं और अभी इसी शरीर में की जा सके। ऐसे व्यक्ति के समक्ष व्यस्त गृहस्थ जीवन में दुविधाएँ आती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने अधिक कार्य दैनिक जीवन में एकत्र हो जाते हैं कि भक्ति-भाव से प्रार्थना एवं आराधना-रूप में आत्मा को अनिवार्य अभ्यास करने का समय ही नहीं प्रतीत होता। यह महानतम विघ्न है; किन्तु यह अधिक गम्भीर नहीं है और न ही प्रमुख है।
आपके सांसारिक व्यावहारिक जीवन के कर्तव्यों की पूर्ति भी प्रमुख विघ्न का कारण रूप है। क्यों? क्योंकि जीवन की सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थ से सम्बद्ध है और जीविकोपार्जन हेतु मनुष्य को कार्य करना पड़ता है। परम्परागत प्राप्त पैतृक सम्पत्ति के दिवस तो अब स्वप्न बन कर रह गये हैं। अब मनुष्य को परिश्रम करना पड़ता है और व्यावहारिक जीवन का यह श्रेष्ठ पक्ष है। गौण पक्ष गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ से दिन-प्रतिदिन मनुष्य कार्यक्षेत्र की ओर अग्रसर होता है और दिन-भर के कार्य की समाप्ति के उपरान्त गृहस्थ में ही प्रत्यागमन करता है। तृतीय पक्ष में, समाज का एक उत्तरदायी सदस्य होते हुए समाज में मनुष्य को विशेष उत्तरदायित्व निभाने होते हैं और क्लब जाना, मित्रों से व्यवहार करना आदि। अन्ततः प्रत्येक मनुष्य का अपना व्यक्तिगत आत्मिक जीवन होता है।
अपना व्यक्तिगत जीवन आधार है। आपके जीवन का अपना व्यक्तिगत पक्ष आपके लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उसके पश्चात् पारिवारिक अथवा गृहस्थ जीवन है जिसमें पति-पत्नी, माता-पिता और सन्तान, भाई-बहन आदि के अनेक सम्बन्ध हैं। तदुपरान्त है-व्यावसायिक जीवन। यह व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः धन की दृष्टि से अपरिहार्य होते हुए भी इसका महत्त्व शून्यवत् है। व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करना आवश्यक है; किन्तु व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। किन्तु वध्यापुरुष (Hangman) और मिलिटरी में काम करने वाले इसमें अपवाद हैं जिनका कार्य मनुष्यों का प्राणान्त करना है और इसके पश्चात् गम्भीर आध्यात्मिक और नैतिक समस्याओं का सृजन करना होता है। किन्तु अधिकांश जनता के लिए व्यावसायिक पक्ष का जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता ।
अधुना, मनुष्य-जीवन के जिन चार प्रतिरूपों का विवरण दिया गया है, उनमें से हमें यह कैसे विश्वास हो कि आध्यात्मिक आदर्श को ही प्रथम स्थान क्यों दिया गया है?
विवाह की पवित्रता
गृहस्थियों को क्षण-भर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि पाणिग्रहण पवित्र संस्कार है। विवाहित जीवन की पवित्रता की अनुभूति इसके पूर्णत्व और पूर्ण गम्भीरता में करनी चाहिए। विवाह एक संस्कार है। यह मात्र दो शरीरों का संयोग नहीं है। यह तो इसका सबसे कम महत्त्वपूर्ण अंग है। पति-पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके पार्थिव जीवन से ऊपर कोई प्रेम ही नहीं है। इससे उत्कृष्टतर प्रेम भी है। सृष्टि के एक रहस्यपूर्ण विधान के अन्तर्गत विवाह दो आत्माओं को ईश्वर की ओर से जीवन-रूपी इस विशाल सूत्र में बाँधने के लिए उसके सत्ता-रूप विशाल स्रोत में लाना है जहाँ असंख्य कोटि आत्माएँ आध्यात्मिक उद्भव के व्यक्तिगत क्षेत्रों में दिव्यता की ओर जाने के लिए विचरण कर रही हैं। भगवान् के आशीर्वाद से, ईश्वर की इच्छा से और इस वैश्विक जीवन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के द्वारा दो आत्माओं का संयोग किया जाता है। विवाह का यही अर्थ है।
इन दो आत्माओं को भगवान् ने इसलिए एक सूत्र में निबद्ध किया है कि वे महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया को कार्यान्वित कर सकें और वह प्रक्रिया है-दोनों का आध्यात्मिक ज्ञान को परस्पर विनिमय करना। पति-पत्नी जो-कुछ धनार्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो भी उनका अध्यात्म-बल है, उन्हें परस्पर आदान-प्रदान करना है। पति को अपनी पत्नी के आध्यात्मिक जीवन को और पत्नी को पति के आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाना है और दोनों को दिव्य बोध की परम प्राप्ति हेतु साथ-साथ आगे बढ़ना है। विवाहित जीवन का सच्चा और वास्तविक उद्देश्य यही है। विवाह पवित्र संस्कार है। इसे साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए। इसके प्रति अशिष् भाव नहीं रखना चाहिए। विवाह एक सन्धि है जिसका उद्देश्य शारीरिक उपभोग से कहाँ बढ़ कर है, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है (यद्यपि एक सीमा तक विवाह का एक उद्देश्य यह भी है)। पति-पत्नी की सन्तति भी आध्यात्मिक होनी चाहिए; क्योंकि वे भूतल पर अवतरित अन्य आत्माएँ हैं जो अपने उद्देश्य के प्रयोजन की पूर्ति हेतु आयी हैं। अतः यह पति-पत्नी का पावन धर्म है कि वे सन्तति के रूप में अवतरित इन आत्माओं को आदर्श गृह तथा समुचित प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करें। शिशु यावत्पर्यन्त बड़े हो कर संसार में बाहर नहीं निकलते, तावत्पर्यन्त उन्हें संरक्षण में रखना अनिवार्य है। शिशुओं का संवर्धन और पोषण उनकी अपनी आध्यात्मिक प्रकृति और आध्यात्मिक उद्भव उनके अपने संचित कर्मों के अनुसार होगा। पुनरपि, माता-पिता अपने जीवन से अपनी सन्तति को प्रारम्भिक आध्यात्मिक विश्लेषण हेतु तब तक पर्याप्त सहायता कर सकते हैं, जब तक वे ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाते कि वे अपने आध्यात्मिक विकास का स्वयं ध्यान रख सकें। यदि बाल्यावस्था में ही उनके मस्तिष्क में पुष्ट आध्यात्मिक विचारों का अध्यारोहण किया जाये तो आने वाले समय में संस्कार अवश्यमेव परिस्फुटित होंगे और सन्तति के लिए परम सुखद होंगे।
विवाह होने तक सन्तान को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराना आवश्यक है, अतएव पति-पत्नी को स्वयं दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और यह सन्तुलित वैवाहिक सम्बन्ध के रूप में होना चाहिए। वैवाहिक जीवन आत्म-संयम पर आधारित होना चाहिए, आसक्ति पर नहीं। पति को पत्नीव्रत एवं पत्नी को पातिव्रत्य का पालन करना चाहिए, पत्नी का किसी अन्य पुरुष से सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। उसे पर-पुरुष का विचार भी नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसकी आसक्ति अपने पति में ही होनी चाहिए। अन्य पुरुष का विचार उसके मन में भूल से भी न आये। सम्पूर्ण मानवता उसके लिए अपनी सन्तान के समान हो। वह जगज्जननी है। राम की भाँति पति को एकपत्नी-व्रत धारण करना चाहिए जिसका अभिप्राय है कि पर-स्त्री का विचार उसके मन में कदापि प्रवेश न करे। उसके लिए एक स्त्री ही उसकी पत्नी है और उनके विवाह-सम्बन्ध पवित्र हैं।
इस प्रकार से सम्पूर्ण पारिवारिक व्यवस्था पवित्र और धार्मिक बन जाती है और जीवन का आन्तरिक जीवन निर्विघ्न आगे बढ़ता है। जीव के बाह्य जीवन में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है जो आध्यात्मिक जीवन को हानि पहुँचाये। बाह्य जीवन के अन्तर्गत पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है जो आध्यात्मिक जीवन में बाधा डाले अथवा उस पर वार करे।
एवंविध, पति-पत्नी दोनों पूर्ण एकता से साथ-साथ चलते हैं और उनके जीवन, बाह्य गतिविधि और आन्तरिक प्रार्थना-भाव के दो पक्षों पर सवार चेतन परमात्मा की आत्यन्तिक आनन्दावस्था भगवद्-साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। वे जहाँ भी रहें, उनके पारिवारिक तथा निजी जीवन में परम आनन्द का वास होता है।
गृह-एक पवित्र स्थान
गृह को पावन स्थान के रूप में देखना चाहिए। आपके दैनिक व्यस्त जीवन में हर प्रकार की भावुकता और अश्रान्त कर्मण्यता में सामंजस्य लाने के लिए गृह एक समीकरण तत्त्व है। जिस क्षण आप गृह त्याग कर व्यावसायिक कर्म हेतु बाहर जाते हैं, आपका सम्पूर्ण मन, आपका समस्त व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। आपको कर्मशील होना पड़ता है। इस संसार के पदार्थों की ओर एकाग्रचित्त होना पड़ता है, इसलिए आपकी स्मृति विलुप्त हो जाती है। आप अपने केन्द्र से दूर पहुँच जाते हैं। जिसके कारण ईश्वर के साथ आपकी आभ्यन्तर आध्यात्मिक सन्निधि का, दैनिक व्यावसायिक कर्म में रत होने के कारण पूर्णतया लोप हो जाता है। अब घर वापस आने पर तो गृहस्थ जीवन एक प्रभावपूर्ण समीकरण तत्त्व होना चाहिए। अपने गृह में आप 'आत्म-केन्द्रित' हैं, समाहित हैं, भगवान् में स्थित हैं। अतः गृह का समस्त वातावरण ईश्वर की विद्यमानता के भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। गृह के प्रत्येक कोण में आपको प्रभु की विद्यमानता का आभास करना चाहिए। एक ऐसा स्थान हो, जहाँ प्रवेश करते ही आपका मन, जो व्यावसायिक, लौकिक कर्तव्यों के कारण प्रसभतः बहिर्मुख हो गया था, पुनः जीवात्मा में आवर्तित हो जाये, भगवान् में विश्राम और शान्ति का अनुभव करने लगे। भगवान् ही घर का प्रमुख होना चाहिए। आप ऐसा अनुभव न करें-"यह घर मेरा है, यह बँगला मेरा है, प्रत्युत यह भगवान् का घर है, यहाँ हमें विश्राम की सुविधा है और मुझे यहाँ मोक्ष के लिए कार्य करना है।" पति-पत्नी दोनों का यही भाव होना चाहिए। बच्चों का उत्थान भी इसी भाव में होना चाहिए।
घर का वातावरण अश्लील नहीं बनाना चाहिए। घर एक ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जो एक प्रकार से दिखावा हो, जहाँ आप अपनी समृद्धि, उच्चतर आस्वादों अथवा सम्पन्नता का दूसरों को दिखावा कर सकें; प्रत्युत इसका अनुष्ठान सरल एवं अनुग्रहपूर्ण ढंग से होना चाहिए जो नम्रता से अलंकृत प्राकृतिक आध्यात्मिकता से युक्त हो और जिसमें इस जागृति-रूप वरदान हेतु प्रभु का धन्यवाद किया गया हो। गृह में प्रापंचिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। घर में सब-कुछ आध्यात्मिक होना चाहिए, यौगिक होना चाहिए। आपके परिवेश में पर्याप्त भौतिकता है, पर्याप्त विस्मरणशीलता और भगवान् के प्रति असावधानी है। अतः आप भी उसमें सम्मिलित हो कर घर के वातावरण को दूषित न करें। घर में भगवान् से सम्बन्ध रखें। घर के परिवेश का प्रत्येक कण पवित्रता से पूर्ण हो और घर के वातावरण को बनाये रखने में यथाशक्ति प्रयास करें। इसे पवित्र रखें। शुद्ध रखें। सदा अनुभव करें कि घर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ आप भगवान् के अत्यन्त समीप पहुँच सकते हैं।
शिशुओं का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शन
शिशु-शिक्षण दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है। माता-पिता के लिए घर एक महान् और दुर्भर (भारी) उत्तरदायित्व है। इन आत्माओं के आप केवल संरक्षक हैं, उनके साथ आपका कोई चिरस्थायी सम्बन्ध नहीं है। प्रभु द्वारा आपको सौंपे गये बच्चों के साथ आपको उस अल्पकाल में ही उनका जीवन और अधिक ज्योतिर्मय बनाने का प्रयास करना चाहिए जितना काल वे आपके संसर्ग में व्यतीत करते हैं। इसी उद्देश्य से वे आपके पास आये हैं। अतः शिशु का समुचित शिक्षण महान् कर्तव्यों में से एक है। और यदि यह सब इस भाव से किया जाये कि आपको प्रभु की ही सन्तति को शिक्षा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो निज सन्तति के प्रति आप जो कुछ भी करते हैं, वह आपके कर्मयोग का अंग बन जाता है। आपके अपने आध्यात्मिक उन्मीलन का अंग बन जाता है; क्योंकि अपने आदर्श जीवन द्वारा उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा, आध्यात्मिक जीवन प्रदान करने से आप प्रभु के जीवन में अंश-भागी बन जाते हैं; क्योंकि आप कर्मयोग के महान् संवाद की पूर्ति करते हैं। दृष्टान्तरूपेण-अनासक्त निष्काम सेवा, हृदय में केवल प्रेम-भाव और परोपकार की भावना। यदि आप उन्हें शाश्वत कल्याण के पथ की ओर अग्रसर करें तो यह महानतम वरदान है जो इस भूतल पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रदान कर सकता है।
शिशु अनुकारक होते हैं। अतएव उन पर सबसे बड़ी दान-वृष्टि स्वकीय दृष्टान्त द्वारा प्रेरणा की दान-वृष्टि है। यह आपका परम कर्तव्य है। घर में माता-पिता को आदर्श बनना होगा। सब परिस्थितियों में उनकी वाणी, उनके कर्म और परस्पर आचार-व्यवहार, उनका चरित्र, पड़ोसी के सम्बन्ध में उनका व्यवहार, उनका सामान्य व्यवहार-यदि वे सब तथ्य आदर्श और गुणों पर आधारित तथा नीति की दृष्टि से परिपूर्ण हैं तो उन्हें अपनी सन्तान को अन्य किंचिदपि प्रदान नहीं करना है। माता-पिता के प्रभाव के प्रकाश में तप कर शिशु अपना सर्वस्व शिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। यह महान् गृह-योग है। शिशुओं को आदर्श वातावरण और आदर्श दृष्टान्त प्रदान करने के लिए उन्हें देने योग्य किसी भी अन्य वस्तु-जैसे पोशाक, अच्छी शिक्षा-आदि से यह कहीं अधिक मूल्यवान् है; क्योंकि ये वस्तुएँ तो आपकी छत्रछाया में पल रही इन आत्माओं के केवल बाह्य स्वरूप का स्पर्श करती हैं। शिशुओं के लिए 'अत्यन्त शीघ्र ही प्रारम्भ' नामक कोई वस्तु नहीं है। एक वर्ष की आयु से ही वे शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक नारियाँ बच्चों को अनुशासित रखने का गर्व करती हैं। तीन मास के बच्चे के लिए माताएँ उद्घोषणाएँ करती हैं- "अहा! वह जानती है, उसे अपना भोजन कब माँगना है। निर्धारित समय से पूर्व चिल्लाती नहीं। वह सब-कुछ जानती है, कब चिल्लाना है और कब नहीं; भोजन कब स्वीकार करना है और कब नहीं। और यदि यह समय से पूर्व ही दीदी द्वारा दिया जाता है तो वह अस्वीकार कर देगी। आप जानते हैं, इसे शिक्षण दिया गया है।" जब आप भोजन की आदतों के लिए शिशु को शिक्षण देने पर इतना गर्व करती हैं, तो प्रारम्भ से ही आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका शिक्षण प्रारम्भ क्यों नहीं कर देतीं? आप उन्हें जन्म से पूर्व ही शिक्षित कर सकती हैं। गर्भ में ही आप इन शिशुओं को धार्मिक विचार, प्रेरणाप्रद आध्यात्मिक तरंगें, भगवान् के प्रति आध्यात्मिक विचार, प्रार्थना और प्रेम के प्रति भावनाएँ प्रेरित कर सकती हैं। तब जन्म से पूर्व ही शिशु उस स्वभाव के अंश को ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार से प्रारम्भ से ही आप शिशुओं को कल्याणकारी रूप में प्रभावित कर सकते हैं।
शिशु को परिवार की प्रार्थना को देखने का अवसर दो। ऐसा प्रार्थना में सम्पूर्ण परिवार एकत्र हो और यदि कोई अतिथि परिवार में रह रहा हो तो उसे भी प्रार्थना में सम्मिलित करो। ऐसी पूजा और भक्ति के लिए प्रातः- सायं नियत समय हो। इस प्रार्थना के समय से पूर्व दिनचर्या प्रारम्भ नहीं होनी चाहिए। इस समय की सृष्टि आपके हाथ में है। यह शीघ्र सोने में है, दूरदर्शन की संलग्नता में नहीं। यह कहना अनिवार्य होगा कि शिशुओं का आध्यात्मिक जीवन अधिकांशतया माता-पिता की असावधानी के कारण नष्ट हो रहा है। माता-पिता कभी ध्यान नहीं रखते कि शिशु क्या कर रहे हैं जब तक कि वे उन्हें तंग न करने लगें। यही तो वे चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि शिशु उसे बाधित करें। यदि वे अपने बच्चों द्वारा बाधित होना भी नहीं चाहते, उनका ध्यान रह रखना चाहते, बच्चों के शिक्षण का उत्तरदायित्व कन्धों पर नहीं लेना चाहते, तो मि उन्होंने बच्चों को जन्म क्यों दिया? उन्हें तो शिशु को जन्म ही नहीं देना चाहिए था। आत्म-संयम करना ही उनके लिए हितकर था। लोगों को चाहिए कि पाणिग्रहण-संस्कार करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। शिशु को जन्म न दें। शिशु को जन्म देना और उसके विकास के प्रति उपेक्षा करना-विशेषतया उसके नैतिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति, इससे बढ़ कर कोई पाप नहीं है; क्योंकि ऐसे माता-पिता ने एक 'विश्वास' के साथ विश्वासघात किया है। अपने ही संकल्प से उन्होंने विश्वास को जन्म दिया और उसके साथ विश्वासघात किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्म-नियम के अनुसार प्रतिफल निश्चित है।
आधुनिक परिवार में आप क्या देखते हैं? अधिकांश बच्चे स्वयं ही व्यसनों का संवर्धन करते हैं। वे माता-पिता से नहीं, प्रत्युत दूरदर्शन के चित्रपट पर से इन दुर्गुणों को ग्रहण करते हैं। यह उनकी आत्माओं को कलुषित करने के समान है। यह उन्हें चित्रपट पर झलकते चित्रों के चक्कर में डालने का दुर्व्यसन है और उनका व्यक्तिगत अस्तित्व पूर्णतया नष्ट करने का साधन है। तब उनके पास किसी अन्य कार्य के लिए समय नहीं रहता। वे सदा दूरदर्शन से ही अभिमन्त्रित रहते हैं।
गृहस्थी के लिए आध्यात्मिक दिनचर्या
प्रत्येक गृहस्थी की एक आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए। गृहस्थ-जीवन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। इसमें अवधान अनिवार्य है। अनपेक्षित घटनाएँ जो प्रतिदिन होती हैं जैसे-आगन्तुक का आगमन, टेलीफोन, किसी के साथ बाहर जाने का निमन्त्रण आदि, इन सबके अतिरिक्त आपका एक मान्य नियमित भौतिक कार्यक्रम होना चाहिए, दैनन्दिन जीवन के लिए एक मौलिक परिशिष्ट होना चाहिए जिसमें प्रातः-सायं एक-एक घण्टा प्रार्थना की वेला भी हो। प्रार्थना की वेला में शास्त्राध्ययन, धार्मिक और प्रेरणाप्रद पुस्तकों का पठन, कुछ क्षण शान्त, अन्तर्मुख ध्यान, कुछ मिनट की वास्तविक परिस्फुटित प्रेरणादायी प्रार्थना समाविष्ट हो। प्रार्थना स्वेच्छानुरूप भी हो सकती है। आवश्यक नहीं कि यह किसी पुस्तक में से ली गयी हो। अथवा यह दोनों प्रकार से हो सकती है।
क्योंकि कभी-कभी अत्यन्त प्रेरणाप्रद छोटी प्रार्थना, किसी संवार्ता अथवा अन्य पुस्तकों से प्राप्त हो जाती है। बच्चों का शिक्षण भी इसी भाँति होना चाहिए।
बाह्य पूजा का भी कुछ वास्तविक अनुष्ठान होना चाहिए। पुनरपि, हम सदेह प्राणी हैं और हमें देह को भी भक्ति में क्रियाशील करना वांछित है। बत्ती जला कर सुगन्धित धूप आदि जलाओ, इष्टदेव को प्रणाम करो, सांजलि अनुनय करो; प्रार्थना करो कि वह आपको ज्योतिर्मय बना दे, आपका हृदय शील गुणों से भर दे, आपके हृदय में दिव्य प्रेम, सात्त्विकता और निष्काम भाव की गंगा प्रवाहित कर दे और तत्पश्चात् घुटनों के बल नीचे झुक कर प्रणाम करो, झुको, मस्तक झुकाओ, एवंविध आपको ईश्वर की विद्यमानता के समक्ष जीवात्मा को नम्र बनाना है। शरीर का घुटनों के बल झुकना, दण्डवत् करना और अपने को विनीत करना आदि अल्प क्रियाओं का मन के ऊपर शुद्ध प्रभाव पड़ता है। शरीर की इन प्रतिक्रियाओं का मन के ऊपर और मन का अन्तरात्मा के ऊपर होने वाले प्रभाव से हम पूर्णतया निरपेक्ष नहीं हो सकते। अतएव, प्रत्यार्ह आपको एक घण्टा नियत करना चाहिए। जब आप अपने अस्तित्व के सभी पक्षों को क्रियाशील कर सकें-जैसे प्रार्थना में शरीर, हृदय और भावों को; अध्ययन में मन और बुद्धि, मनन और प्रश्न-"मैं कौन हूँ", अन्तः- ध्यान, मौन, अन्तर्मुखता और ध्यान में आत्मा को क्रियाशील करना।
परिवार के सभी सदस्यों का निजी पूजा-स्थान नियत होना चाहिए। माता का एक कोने में अपना स्थान होना चाहिए, जहाँ वह अपनी छोटी-सी प्रार्थना, भगवान् से छोटा-सा वार्तालाप, पथ-प्रदर्शन हेतु प्रार्थना और घनिष्ठ संसर्ग स्थापित कर सके। एवंविध, पति का भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए और यदि ऐसा सम्भव न हो, तो कम-से-कम उसके पास अपने लिए कुछ समय होना चाहिए, जब वह विधाता के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद कर सके। प्रारम्भ से ही बच्चों को अपना-अपना स्थान ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। जिस प्रकार उनके खिलौनों के लिए कोण नियत रहता है और द्वितीय उनकी पुस्तकों के लिए तथा अन्य उनके मित्रों के लिए इसी प्रकार सर्वोच्च अस्तित्व के साथ सम्भाषण हेतु भी उनका एक पृथक् स्थान होना चाहिए। यदि शैशवकाल से ही यह स्वभाव बना लिया जाता है, तो पश्चात्काल में वे अपना स्वतन्त्र आध्यात्मिक जीवन बनाने में समर्थ हो जायेंगे।
क्रियाशील आध्यात्मिकता-भगवद्-स्मरण
सम्पूर्ण गृह में कुछ ऐसे बाह्य चिह्न रखने चाहिए जो भगवान् का स्मरण कराते रहें। कदाचित् वे आवेष्ठित आदर्श वाक्य हों जैसे-"सर्व जीवन पवित्र है", "ईश्वर यहीं अभी आपके साथ है", "अच्छे बनो, अच्छा करो", "दयालु बनो, पवित्र बनो, सत्य बोलो", "किसी की भावनाओं को आघात न पहुँचाओ", "सब प्राणियो में भगवद्-दर्शन करो", "सत्य भगवान् है", "प्रेम भगवान् है", आदि। चित्र भी टाँगने चाहिए। व्यवसाय हेतु बाहर जाने से पूर्व प्रतिदिन गृहस्थी को पाँच मिनट तक प्रार्थना करनी चाहिए- "हे प्रभु, आपके इस आनन्दमय धाम से, जहाँ मुझे अपने दिन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं कार्यरत हो कर शारीरिक कृत्यों द्वारा आपकी उपासना करने बाहर जा रहा हूँ। मैं शरीर और मन से जो भी कार्य करूँ, उसे आप पूजा-रूप में, कर्मयोग-रूप में, सशक्त प्रार्थना के रूप में स्वीकार करें।" यह छोटी-सी प्रार्थना बोलने के उपरान्त ही गृहस्थी को घर से बाहर पग रखना चाहिए।
कार्यालय पहुँचने पर आपको उपासना-भाव ऐसा करना चाहिए। आप स्टेनो-टाइपिस्ट हों, विक्रेता हों अथवा औषध-भण्डार के सहायक हों, चिकित्सक हों, वकील हों अथवा विद्यालय के अध्यापक हों, बढ़ई हों, मिस्त्री हों, कुछ भी हों, आप जिस स्थान पर कार्य अथवा व्यवसाय हेतु प्रतिदिन जाते हैं, वह स्थान आपके लिए भगवान् का पवित्र मन्दिर होना चाहिए और आपका कार्य उस सर्वव्यापक सत्ता को अर्पित अर्चनांजलि हो जो घर में है, भीतर है, सर्वत्र है और जो आपके कार्यालय में भी विद्यमान है।
यदि आप दुकानदार हैं, तो धनार्जन पर आपको ईश्वर के साथ कार्य करना चाहिए। आपको ऐसा अनुभव हो कि ईश्वर आपके साथ कार्य कर रहे हैं और यदा-कदा, लगभग घण्टे में एक बार, आपको यह भाव पुनः जागृत करना चाहिए। यह समरूप और यन्त्रवत् नहीं होना चाहिए और न ही कुण्ठित होना चाहिए। भाव को पुनः जागृत इस प्रकार करना चाहिए- "हे प्रभु, इस कार्य को अपनी अर्चना मान कर स्वीकार करो। सर्व महिमा आपकी है। आपकी ही कृपा से मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं आपको यह कर्म समर्पित करता हूँ जैसे समाधि पर पुष्प अर्पित किये जाते हैं।"
यदि आप बन्दी-गृह में कार्य करते हैं अथवा आप वकील हैं और मानो 'तलवार की धार' पर कार्य करना पड़ता है, तो यह करना अत्यन्त कठिन है। वकील बन कर तो असत्य न बोलना अत्यन्त कठिन है, रक्षापुरुष (सिपाही) हो कर रिश्वत न लेना कठिन है। ऐसे कार्यों में लोग दया के पात्र हैं; क्योंकि वे मनुष्य-जीवन-रूपी अमूल्य वस्तु को व्यर्थ खो रहे हैं। वे स्वयं भी अत्यन्त दुर्भाग्यशाली हैं; क्योंकि वे ऐसे जाल में बंध जाते हैं जहाँ वे इच्छा न होते हुए भी अनैतिक, अधार्मिक कृत्य करते हैं। पुण्यात्मन् आध्यात्मिक साधक को इन व्यवसायों का परित्याग कर देना चाहिए। अन्यथा आपको अत्यन्त सावधानी से और भगवान् के प्रति भक्तिवत् हो कर उसे निरन्तर प्रार्थना करते हुए कार्यरत रहना चाहिए कि वह आपको सुपथगामी बनाये। पूजा में सर्वस्व भगवान् को ही अर्पण करना होता है और पूजा दूषित नहीं हो सकती, कपट-भाव से युक्त नहीं हो सकती, अशुद्ध नहीं हो सकती; अतः आपके जीवन को अनुशासित करने वाला एक ही नियम होना चाहिए कि यह निष्कपट और सत्य पर आधारित हो। आपकी सर्व क्रियाएँ सत्य, ईमानदारी और पवित्रता पर आधारित होनी चाहिए। तब वही क्रियाएं भक्ति-भाव से भगवान् को समर्पित किये जाने पर योग बन जाती हैं। वे कहीं भी योग बन जायेंगी-पेरिस हो या लन्दन, न्यूयार्क हो या वैन्कुवर। समय अथवा युग जिसमें आप वास कर रहे हैं, बीसवीं शताब्दी हो अथवा पच्चीसवीं, इसका विशेष महत्त्व नहीं। जिस स्थान पर आपका वास है वह पूर्व हो अथवा पश्चिम, इसका भी बहुत कम महत्व है। महत्त्व इस बात का है कि आप सब कार्यों को पूजा की दृष्टि से लें और ध्यान रखें कि आपके सर्व कर्म सदाचार, सत्य और पवित्रता के नियमों पर आधारित हों। एवंविध आपका सम्पूर्ण जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका गृहस्थ-जीवन और कार्यालय का व्यावसायिक जीवन योग के भाव से व्याप्त हो जाता है।
भोजन की वेला में मौन आन्तरिक प्रार्थना और अन्तर्ध्यान के लिए पन्दरह मिनट खींचने का प्रयास करो। अपने-आपसे दूर हो जाओ। यदि ऐसा करने में आप संकोच अनुभव करते हो, तो कहीं एक ओर आसनस्थ हो कर समाचार-पत्र पढ़ने का बहाना बना कर समाचार-पत्र की ओट में उन क्षणों में भगवान् पर ध्यान करो अथवा एक झपकी (स्वल्प निद्रा) लेने का व्यपदेश (बहाना) करो। नेत्र बन्द करो और ध्यान में उतरने का यत्न करो। परन्तु वास्तव में निद्रा न करो। पूर्णतया भगवान् पर एकनिष्ठ होते हुए संसार को विस्मृत करो। जीवन, कार्य, शरीर आदि सर्वस्व उस क्षण के लिए विस्मृत कर दो। यह एक शक्तिपूर्ण प्रक्रिया है। यदि आप अपने अन्तस्तम अस्तित्व में यदा-कदा डुबकी लगायें-दिन में बीस बार, प्रत्येक आधा घण्टे में एक बार और वह एक मिनट के लिए भी हो तो पर्याप्त है। यह जीवन को रूपान्तरित करने की एक महान प्रक्रिया है। यह सशक्त आध्यात्मिकता है और जो रूपान्तरण आयेगा, उसमें आप किसी भी ध्यानस्थ यति से आध्यात्मिक परिवर्तन में कम न होंगे; क्योंकि आपका कार्य उस यति के कार्य से कहीं अधिक दुष्कर है। उसे तो सब समुचित सुविधाएँ प्राप्त है। इसलिए उसके लिए ध्यानस्थ होना स्वाभाविक और सरल है; किन्तु सब-कुछ आपके विपरीत होते हुए-जब सम्पूर्ण वातावरण, सम्पूर्ण परिसर, सभी तत्त्व जो आपके जीवन के निर्माता हैं, सर्वथा भौतिक हों, बाह्यगत हों और स्थूल रूप से प्रापंचिक हों-और यदि इन सबके मध्य में आप क्षण-भर के लिए अन्तर्मुख होने का विचार करते हैं, तो आपका ईश्वर-प्रेम का लक्षण इतना सत्य और गाढ़तः यथार्थ होगा कि उसकी फल-प्राप्ति दश-गुणित, शत-गुणित होगी। अतः अपने व्यस्त दिवस में समय-समय पर गहन और अनन्यमनस्क भगवद्-चिन्तन हेतु कतिपय क्षण निकालने का प्रयास करें। यथासम्भव प्रत्येक वस्तु को भगवान के साथ सम्बद्ध करें। जो कुछ भी करें, प्रभु-प्रेम में करें और अपने कर्मों में तथा कमाँ के द्वारा उससे सम्भाषण करने का प्रयास करें।
आप यदि जलपान-गृह में सेवक हैं, तो सेवा के समय आदेश देने वाले मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करें और पूजा-भाव से उसे भोजन दें मानो आप भगवान् को भेंट चढ़ा रहे हों। उस समय के लिए ग्राहक की मेज आपका पूजा-स्थल बन जाये। इस प्रकार से आपकी प्रत्येक क्रिया भगवद्-चिन्तन से सम्बद्ध हो और आपका हृदय भक्ति से भरपूर हो (इसे भावुकता की भ्रान्ति में नहीं लेना है, प्रत्युत यह पूजा-भाव की वास्तविक स्थिर अवस्था को प्रतिपादित करती है। निर्बलता नहीं, बल ही सच्ची भक्ति का लक्षण है)।
फैशन का अभिशाप
इतना सब करते हुए सादा जीवन व्यतीत करें। सरल जीवन में ही मन स्थिरता से सुपथ पर चलता है। यदि जीवन नानार्थक है, असरल है और विषय-संग्रह की भावन से पूर्ण है तो मन विक्षिप्त और असंहृत होने लगता है। सरल जीवन व्यतीत करें औ अपने भौतिक अस्तित्व, शरीर, सज्जा, सौन्दर्य एवं पोशाक की ओर अधिक ध्या न दें।
यह एक सहज सत्य है कि फैशन अभिशाप है। फैशन अभिशाप भी है अ दासता भी है। उन चतुर जनों की आप दासता करते हैं जिन्होंने अपने उत्पादन विक्रय करना है। बुद्धिमत्ता से विचार करने पर आपको अत्यन्त गम्भीर और महत्त्व तथ्य का ज्ञान होगा; पोशाक अथवा अन्य फैशन की सामग्री के निर्माता एक विशेष और स्वरूप की वस्तु एक वर्ष की अवधि से अधिक निरन्तर अपने पास नहीं रस निश्चयेन प्रत्येक वर्ष वे नये फैशन में नये मॉडल में परिवर्तन लायेंगे और आपक बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि गत वर्ष आपने जो वस्तुएँ खरीदीं, वे अब निरर्थन क्या आप इस निरर्थकता की ओर दृष्टिपात करते हैं? फैशन की दासता जीवा असीम संकीर्ण बना देती है। सरल जीवन से हृदय सरल, मन सरल रहता है औ अपना हृदय और मन भगवान् को अर्पण करने योग्य हो जाते हैं। संकीर्ण जीवना और हृदय विक्षिप्त हो जाता है और अनिवार्य आन्तरिक जीवन लुप्त हो जाता है ।
समय का मूल्य
समय का मूल्यांकन करो। प्रत्येक क्षण का उपयोग करो और अत्यन्त कृपणता से करो। प्रत्येक क्षण समुद्धृत करो और अपने आध्यात्मिक जीवन में इसे जोड़ दो। वृथा संलाप, गप-शप आदि का अनुशीलन न करो। यह एक सामाजिक गुण है कि जब भी दो मनुष्य समवेत हों, वे किसी तृतीय पुरुष की निन्दा करते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं, तो आप अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और समय वृथा खो रहे हैं। जीवन समय है और समय ही निश्चयेन जीवन है। यदि आप अमूल्य क्षणों तथा वेला को वृथा संलाप और निरर्थक बातों में खो देते हैं, तो इसका आशय है कि आप जीवन की अमूल्य वस्तु-भगवद्-प्राप्ति के दुर्लभ सुअवसर से स्वयं को वंचित कर रहे हैं।
थोड़ा साहसी बनने का प्रयास करो। अन्य जनों से पृथक् होने में आपको भय नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए- "यदि मैं इस प्रकार का हूँ, यदि मेरी गृहस्थी अमुक प्रकार से चलायी जाती है और पड़ोसी झाँकते रहें तो वे क्या सोचेंगे।"
वे कुछ भी सोचें, आप उनकी परवाह क्यों करते हैं? उन्हें जैसा रुचिकर लगे, सोचने दो। आप किस बात की चिन्ता करते हैं-भगवद्-चिन्तन की, निजात्मा की अथवा लोकमत की? दृढ़ निश्चय रखो। कुछ बातों में विशिष्ट बनने का और सामान्य से ऊपर उठने का साहस करो। ऐसा मत सोचो कि आपको सदा (प्रत्येक तथ्य) प्रभावित करना है। जनगण के सामाजिक कल्याण हेतु अनिवार्य तथ्यों को दृढ़ करना चाहिए; किन्तु आभ्यन्तर जीवन में किसी के दृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं। वही करो जो परमेश्वर की दृष्टि से आपको सर्वोत्तम प्रतीत होता है। आपका कुछ स्वतन्त्र चिन्तन होना चाहिए और अपना पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन ऐसे ढंग hat H व्यतीत करो जो आपको सर्वोत्तम प्रतीत हो, उच्चतम आदर्श के अनुकूल हो।
संक्षेप में, यह विधि विहित है जिसके द्वारा आप अपने समस्त जीवन में आध्यात्मिक तत्त्व का विकास कर सकते हैं। आप पूर्वीय हों या पाश्चात्य, आधुनिक हों अथवा पुरातन, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं। व्यक्ति जहाँ भी हो, इस पूजा-भाव से अपनी अन्तस्तम सत्ता का स्पर्श कर सकता है और निरन्तर भगवान् की ओर प्रेरित करने वाले नियमों को अपना जीवनाधार बना सकता है। आप जो कुछ भी करें, भगवान् की ओर बढ़ें। आपके सर्व कर्म ऐसे हौं जो आपको भगवान् के समीम ले जायें।
उपसंहार
जीवन में नियमित रूप से धर्माचरण का संवर्धन करो। धर्म ही ऐसा मापदण्ड हो जिससे अपने सब विचारों को, कर्मों और वाणी को परख सकें। यह धर्मानुकूल है अथवा नहीं? जीवन में आपके पथ-प्रदर्शन हेतु यह मापदण्ड होना चाहिए। और नियम सदा परमात्मा की ओर अग्रसर होने का होना चाहिए।
पारिवारिक परिशिष्ट में विचारणीय कुछ विषय हैं-कुछ क्षण मौन मनन और परिवार के सदस्यों में विचारों का आदान-प्रदान, कुछ क्षण सार्वजनिक आध्यात्मिक अध्ययन और कुछ क्षण सम्मिलित स्तोत्र-गान। सब परिवारों में सम्मिलित हो कर गाने की प्रथा होनी चाहिए-वे कुछ कण्ठस्थ भजन अथवा स्तोत्र आदि हों।
सदा नियमित रूपेण ब्रह्मार्पण करने के उपरान्त ही स्वयं भोजन ग्रहण करो। भोजन से पूर्व भगवद्-कृपा का स्तुति-गान करो।
गृहिणी को घर का कार्य करते समय सर्व कार्य भगवान् को अर्पण करने चाहिए चाहे वह बरतन धोने का कार्य हो, फर्श पोंछने अथवा भोजन बनाने का कार्य हो। उसे कहना चाहिए- "हे प्रभु! तुम्हारे स्नेह, तुम्हारी महिमा-गान के लिए यह अर्चना है।" और हाथ प्रेम से अपना कार्य करें जिससे आप अनुभव करें कि हाथ और हृदय दोनों परमेश्वर को समर्पित हैं।
अपने सहवासी के साथ आदर्श सम्बन्ध स्थापित करो। आपको एक अच्छा सहवासी (पड़ोसी) बनना चाहिए और परिवार के सब सदस्यों को सहायक अथवा दानी स्वभाव का होना चाहिए। यदि कोई विपत्ति आ जाये अथवा सहायता का अवसर प्राप्त हो, सहायता की प्रार्थना न भी की गयी हो, यदि आप सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति कष्ट में है, तो स्वयं को अभिव्यक्त किये बिना ही आपको सहायता करनी चाहिए। यदि आप दान देना चाहते हैं, अथवा एक अच्छे दानी का आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनेक विधियाँ हैं। इसे आप आज ही कर सकते हैं। जीवन में इनका स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। अतः ईश्वर की उपासना करो और योग, दया, सदाचार और निष्काम भाव के आदर्श को अपने सहमित्रों के साथ व्यवहार में पूर्ण करो।
सप्ताह के अन्तिम दिवस मनोरंजन अथवा आध्यात्मिक मनोरंजन के हों। सप्ताह के अन्तिम दिनों में विहार की लालसा क्यों बनी रहे? बच्चे बाहर क्यों जाना चाहते हैं? यदि घर का वातावरण इतना आदर्श और सुन्दर बन जाये, सुख और माधुर्य से परिपूर्ण हो जाये, तो घर का कोई भी सदस्य बाहर जाने की आकांक्षा नहीं करेगा। आपको घर में परिवार के साथ प्रत्येक क्षण प्रेमपूर्ण प्रतीत होगा। आप बहिर्गमन की इच्छा नहीं करेंगे। जब पारिवारिक वातावरण पूर्ण रूप से असात्त्विक हो जाता है और ईश्वर में विश्वास नहीं रहता, उसकी विद्यमानता में आस्था नहीं रहती, भक्ति का अभाव होता है, प्रेम और दान नहीं होता, पति-पत्नी में परस्पर अवधारणा नहीं होती, माता-पिता और सन्तान में सद्भाव नहीं रहता, तब सन्तान अच्छी नहीं हो सकती और ऐसा होने पर वे अननुवर्तिन् और प्रमत्त बन जाते हैं। और यदि घर आदर्श है, स्नेहभावपूर्ण है, पारिवारिक जीवन का केन्द्र भगवद्-प्रेम है, तो कोई भी परिवार घर से बाहर जाने का इच्छुक न होगा और घर में व्यतीत किया गया समय ही आध्यात्मिक उपलब्धि से परिपूर्ण वास्तविक सप्ताहान्त होगा जिसमें आप अपने लिए ऐसा धनार्जन करते हैं जिसको शलभ खा नहीं सकता, धूल नष्ट नहीं कर सकती और चोर चुरा नहीं सकता। इस प्रकार यौगिक जीवन व्यतीत करने से उपलब्ध आध्यात्मिक सम्पत्ति का अग्न्यस्त्र विनाश नहीं कर सकता।
मेरे विचार में, इतना ही, न्यूनाधिक परिवार और गृह में जीवन की यौगिक कला के सम्पूर्ण स्वरूप का सारांश है।
१०. कर्म और पुनर्जन्म
ज्योतिर्मय अमर आत्मन् ! कर्म और पुनर्जन्म का विषय इतना गम्भीर है कि यह प्रत्येक की अवधानपूर्ण विचारणा और बुद्धिमत्तापूर्ण समीक्षा की अपेक्षा रखता है; क्योंकि इसी में उस विधान के सत्य स्वरूप का नियम निहित है जो ब्रह्माण्ड में हमारी सत्ता को संचालित करता है। सामान्यतः जनगण इस विषय के प्रति 'भारत का कर्मवाद' अथवा 'हिन्दूमतानुसार पुनर्जन्म' आदि कह कर असम्बद्ध व्याख्या करते हैं। यह असंगत नाम है। यह किसी सिद्धान्त का निर्माण नहीं, प्रत्युत नियम कां उन्मीलन है। यह ज्ञान रुचिकर है; क्योंकि यह नियम पूर्वीय लोगों की ही विशेष पूँजी नहीं है, प्रत्युत सर्व धर्मों का मूल है और व्यावहारिक रूप में संसार के सब धर्मों ने समान रूप से इसे ग्रहण किया है। एवंविध, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का नियम नहीं है, वैसे ही कर्म और पुनर्जन्म का नियम हिन्दू-नियम नहीं है। नियम के ऊपर न्यूटन का कोई अधिकार नहीं था, यह उसकी पूँजी नहीं था- उसने तो मात्र इसकी क्रिया का अध्ययन करके इसकी उद्घोषणा की। इसी प्रकार से आर्कमिडीज का नियम न तो ग्रीक-नियम है और न ही ग्रीक-अन्वेषण। आर्कमिडीज के अनुसन्धान के उपरान्त ही इसने कार्य प्रारम्भ नहीं किया, प्रत्युत यह सदा से क्रियाशील था और उसी प्रकार से कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त का पूर्व में जन्म नहीं हुआ। इसका अस्तित्व तो आदिकाल से है। मानवता के इतिहास में किसी काल-विशेष में जन किसी ऋषि अथवा मुनि को इसका बोध हुआ अथवा उसके ध्यान में इसका उन्मीलन हुआ और उसने मानवता को इसका ज्ञान दिया, उससे पूर्व ही यह सिद्धान्त सत्ता में था।
अब, इस सिद्धान्त की प्रक्रिया चिरकालपूर्व हिन्दुओं को गहन ध्यान में स्पष्ट की गयी। प्रश्न उठता है- “बीसवीं शताब्दी के प्रगतिशील आधुनिक लोग इस सिद्धान्त को मान्यता क्यों दें? सम्भव है, शताब्दियों पूर्व यह हिन्दुओं के लिए हृदयग्राही रहा हो; किन्तु एक पुरातन सिद्धान्त आधुनिक संसार में व्यावहारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कैसे हो सकता है?" सर्वप्रथम, यह हिन्दू-सिद्धान्त नहीं है। हिन्दुओं को इससे कुछ नहीं करना था। यह ईश्वर का निमय है। ईश्वर ने ब्रह्माण्ड को संचालित करने वाले नियमों की रचना की। और भी, यह पुरातन असामयिक नियम नहीं है जो अब सप्रभाव न हो। यह तो सार्वभौमिक नियम है जो नित्य अमोघ है। यह स्वयं भगवान् का नियम है।
चिरकाल पूर्व प्राणिशास्त्रज्ञों ने अन्वेषण किया कि शारीरिक जीवन के लिए श्वासोच्छ्वास अनिवार्य है। अब मनुष्य यह नहीं कह सकता कि यह तथ्य अब और अधिक मूल्यवान् नहीं है; क्योंकि इसका प्रकटीकरण दीर्घकाल पूर्व हुआ था। जब तक मनुष्य सदेह प्राणी है, वह श्वासोच्छ्वास के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्वास ही उसके जीवन को पुष्ट करेंगे और आक्सीजन अनिवार्य होगी। आक्सीजन के बिना उसकी मृत्यु हो जायेगी। नियम सजीव ही है और प्राणवायु से सम्बद्ध है।
विधान एवं उसकी उपलक्षणा
कर्म और पुनर्जन्म की यह व्याख्या चकित करने वाली भी नहीं है। इसे समझने अथवा स्वीकार करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं। अभी भी यह नियम दृढ़ निश्चय के साथ महान् वैज्ञानिकों द्वारा समझा और स्वीकार किया जा रहा है और ऐसे शब्दों में इसे स्पष्ट किया गया है जो प्रत्येक युक्ति के लिए सुज्ञात हैं। नियम की व्याख्या के अनुसार भौतिक जगत् तक सीमित प्रत्येक कर्म की एक अनुरूप प्रतिक्रिया होती है और प्रत्येक कारण के पीछे एक अपरिहार्य कार्य रूप होता है। प्रत्येक रसजु, प्रत्येक वैद्य का यह मत है कि यह नियम भौतिक वस्तु पर शासन करने वाले बाह्य जगत् में क्रियाशील होता है। यह वही नियम है जिसका उन्मीलन भारत के ऋषियों ने धर्म, नीति और आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्राक्काल में किया था। जिस प्रकार अपने चारों ओर के संसार में हम देखते हैं कि प्रत्येक कारण का एक अपरिहार्य प्रभाव होता है और प्रत्येक कर्म की एक विशेष प्रतिक्रिया होती है। उसी प्रकार से धार्मिक और नैतिक क्षेत्र में प्रत्येक कारण एक विशेष प्रक्रिया को जन्म देता है; बोया हुआ प्रत्येक बीज एक विशेष फल का कारण होता है अथवा अनुकूल शस्य प्रदान करता है। कर्म के सिद्धान्त की सरलतम व्याख्या है : "जैसा बोयेंगे, वैसा पायेंगे।" वैज्ञानिकों द्वारा निरूपित और भौतिक वस्तुओं पर प्रयुक्त सिद्धान्त है- “प्रत्येक कारण एक कर्म होता है और प्रत्येक कर्म की एक अनुरूप प्रतिक्रिया होती है।" इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि 'प्रत्येक कारण एक कार्य को जन्म देता है जिसकी प्रकृति उसके कारण के अनुरूप होगी जिसने उसे जन्म दिया है।' यह अत्यन्त तर्कयुक्त स्वीकृत मत है। भारत में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि 'व्यक्ति का आचार-व्यवहार उसके मन के अनुरूप होता है और विपर्येण मन की प्रकृति उसके भूत कर्मों के अनुरूप होती है।’
मानव-जीवन के लिए यह कर्म का सिद्धान्त अनेक व्यावहारिक परिणामों का स्तम्भ है और इनके सम्बन्ध में अनेक मिथ्यावाद प्रचलित हो गये हैं। इनमें से एक मिथ्यावाद यह है कि जैसे यह नियम मनुष्य के जीवन में अपना कार्य करता रहता है, उसके स्वकर्म की स्वतन्त्रता की अनिवार्यता प्रतिरुद्ध हो जाती है; क्योंकि कर्मगति के अनुसार जो होता है, वह होना ही है और वह अपरिहार्य है तो मनुष्य कर्म कर कैसे सकता है?
अब, जैसा कोई बोता है वैसा ही पाता है। इस विधान की यह उक्ति मात्र भी मनुष्य की रचना का कारण बताती है; क्योंकि कर्मक्षेत्र में मनुष्य ही बीज डालता है। अतः नव बीजों की शस्य भी वही काटता है जो उसे भविष्य के कर्म की ओर ले जाती है। यदि मनुष्य स्वतन्त्र कर्ता नहीं है तो कर्म का विधान ही अनर्थक हो जाता है। यह एक गम्भीर प्रश्न है जिसे हमें समझना है। कर्म का विधान मनुष्य को विधि के अन्तर्गत असहाय पुतली नहीं बनाता ।
हिन्दू कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख-दुःख भोगता है-ऐसा विधि का विधान है और इस सुख-दुःख से आप पलायन नहीं कर सकते। यह विचार उस विचार से किस प्रकार संगतियुक्त हो सकता है कि मनुष्य को स्वतन्त्रता प्राप्त है? हमें नियम को इस प्रकार से अवबोध करना है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दो तत्त्व कार्य करते हैं। एक तो वह अनुभव जो मनुष्य को सहना है और उस पर आने वाले सुख और दुःख, विपत्ति (दुर्भाग्य) और हानियाँ जो उसे सहन करनी हैं। यह अनुभव अपरिहार्य हैं। इनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इन्हें सहन करना ही होता है। किन्तु अन्य तत्त्व है जो मनुष्य के करने वाले (वर्तमान) कर्मों से सम्बद्ध है। यह कर्म व्यक्ति-विशेष की इच्छा पर निर्भर होते हैं।
कर्मानुभूति में तो उसे कोई मनोबन्ध प्राप्त नहीं; किन्तु कर्म करने में वह स्वतन्त्र है। इस सीमा तक वह स्वतन्त्र कार्यकर्ता है। सामाजिक पारम्परिक, सदाचार आदि सम्बद्ध भूतल के अनेक अनुबन्धों के कारण वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र न हो, ऐसा सम्भव है; किन्तु यह प्रमाणित करने के लिए अन्वीक्षिकी (आत्मविद्या) में प्रवेश करना व्यर्थ है। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र कर्ता नहीं है और कर्म का विधान भी अस्तित्व में है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य स्वेच्छा से जो-कुछ भी करना चाहे, कर ले; अपितु वह अपनी इच्छा को क्रियान्वित कर सकता है और इस क्रिया में मनुष्य स्वतन्त्र है। जीवन के अनुभवों के प्रति उसे कोई स्वतन्त्रता, वरण अथवा विकल्प प्राप्त नहीं है; किन्तु अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए एक सीमा तक उसे स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है।
त्रिविध कर्म
इस नियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रतिपादित होने वाले कर्मों को तीन विभागों में बाँट दिया गया है। प्रथम विभाग में कारण और कार्य रूप वैज्ञानिक नियम लागू करने से ऐसा दृष्टिगत हुआ है कि मनुष्य के जीवन काल में कुछ कर्मों का तो तात्कालिक फल प्राप्त होता है, कुछ का वर्षों पश्चात् और कदाचित् अन्य कतिपय कर्मों की इस जीवन-काल में सर्वथा फल-प्राप्ति नहीं होती। उस कर्म का क्या होता है जो इस जीवन-काल में फलीभूत नहीं होता? ऐसे कर्मों का प्रताप, उनकी मानो पुनः क्रियाशील होने की शक्ति जो अनिश्चित कारणों से प्रत्येक मनुष्य के कर्म-भण्डार (कोष) में संचित होती रहती है। यह कर्मों के बीज की प्रथम विधि है।
दूसरी विधि इस प्रकार है-पुनः क्रियान्वित होने वाले कोष में एक भाग मधुर एवं कटु अनुभवों के रूप में कार्यान्वित करने के लिए जीवन के एक समय-विशेष के लिए ले लिया जाता है। वह स्वयं उस विशेष अवतरण में मानो अनुभवों का बीज बनाता है। वह संचय मनुष्य की जन्म-मृत्यु का, उसके सुख-दुःखों का और वह सब जिस पर वह अश्रुपात करता है, इन सबका निर्णय करता है। संक्षेप में वह जो कुछ भी फल भोगता है, वह उस संचित कर्म के फलस्वरूप होता है। यह द्वितीय वर्ग है।
और तृतीय कौन-सा है? इस पार्थिव जीवन में मनुष्य कर्म को उत्तेजित करता रहता है। वह सोचता कुछ और है, करता कुछ और है और इस विशेष पार्थिव जीवन की क्रिया नव-बीज बनाने में सहायक होती है। भविष्य में कभी उसे इस क्रिया का परिणाम भोगना पड़ता है। यह नवीन कर्म किस वर्ग से सम्बद्ध है? स्वभावतः, यह न तो इस जीवन के अनुभवों से सम्बद्ध है और न ही संचित कर्मों से। यह तो नव-कोष से सम्बद्ध है और यह तृतीय वर्ग है। इसमें वर्तमान की क्रियाएँ आती हैं जिन्हें 'क्रियमाण' अथवा 'आगामी' कर्म भी कहते हैं; क्योंकि जो आने वाला है (आगामी है), वह वस्तुतः वर्तमान में प्रकाश में आने वाले कर्म का फल है। अतएव कर्म त्रिविध है-संचित, प्रारब्ध (संचित कर्मों का वह भाग जिसका फल प्रारम्भ हो चुका है) और क्रियमाण कर्म।
इस जीवन में किये जाने वाले कर्मों के दो पृथक् परिणाम होते हैं। एक का तो फल इसी भूतल पर तत्काल ही दूसरे दिवस अथवा आगामी सप्ताह अथवा दस वर्ष पश्चात् प्राप्त हो सकता है; किन्तु मन पर उसकी छाप क्षणिक होती है। किये हुए कर्म-फल का मन अचिरेण ही संस्कार प्राप्त कर लेता है। यदि कठोर और क्रूर कर्म किया जाता है तो कठोरता और क्रूरता का संस्कार मन के ऊपर तत्काल ही चित्रित हो जाता है। पुनः पुनः कृत संस्कार मन में विविध भावों को जन्म देते हैं और वे मन को एक विशेष गुण प्रदान करते हैं। इस प्रकार मन की इन संवर्धित वृत्तियों (भावों) द्वारा बने संस्कारों के गुणों के संचय से व्यक्ति का स्वभाव बनता है। प्रायः इसे मनुष्य का चरित्र कहा जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को कर्म के बाह्य फल से विशेष सम्बन्ध नहीं, प्रत्युत जो संस्कार मन में कर्म द्वारा उत्पन्न होता है, उससे अधिक सम्बन्ध है। क्यों? क्योंकि यह संस्कार मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति बनाते हैं और भावी फसल (परिणाम) की अग्रिम सूचना प्रदान करते हैं?
अब, जिस प्रकार शस्य काटने के लिए वापक को अपने त्रिविध कर्मों का फल भोगने के लिए भूमि पर अवतरित होना पड़ता है। एवंविध कर्मफल भोग के लिए आत्मा पुनः पुनः शरीर धारण करता है। जब तक कर्मों के कारण विद्यमान हैं, नियमानुसार उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता भी है। मनुष्य जब ऐसा साधन खोज लेता है जिससे वह नवीन कारण जन्म नहीं लेते, तब कदाचित् जीवनों के एक क्रम के उपरान्त कर्मों का भण्डार क्षीण हो जाता है और इसके पश्चात् वह एक ज्योतिर्मय अवतार रूप में अवतरित होता है जिसमें उसके और अधिक संचित कर्म शेष नहीं रह जाते। ऐसा सामान्यतया नहीं होता; क्योंकि मनुष्य अपनी राशि को कभी क्षीण नहीं होने देता, इसमें और ही संचित कर रहा है और यह मानव की महान् मूर्खता है।
मनुष्य-स्वयं भाग्य-निर्माता है
क्या यह एक महान् नियम है, अभिशाप है अथवा वरदान है? यह मिश्रित है। अन्ततोगत्वा, यह एक महान् वरदान है। लोगों का इसकी ओर एक ही कोण से देखने का स्वभाव है और वह कोण यह है कि जब तक मनुष्य इस चक्र के बन्धन में पड़ा रहता है, उसे सुख-प्राप्ति नहीं होती, वह दुःखी रहता है और आँसू बहाता है। इस विचार से कर्म सर्वदा मनुष्य के लिए बाधक होगा और कर्म का विधान परमेश्वर के हथौड़े की भाँति उस पर सदा रहेगा। और अविरत कष्टों की वृष्टि करेगा। किन्तु क्या यह स्पष्ट नहीं है कि उसके कर्म का विधान वस्तुतः मान प्रतिकार और दण्ड का नहीं है? इसका एक अन्य गौरवशाली दृष्टिकोण भी है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पाप कर्मों के प्रतिफल से मुक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार से वह पुण्य कर्म फल से भी नहीं बच सकता। सम्पूर्ण विश्व भी उसके अधिकृत पुरस्कार से उसे वंचित नहीं कर सकता। मनुष्य के पुण्य कर्म सदा उसका अनुसरण करते हैं और उसकी महानतम विपत्ति और शोक में रक्षा करते हैं और सुख-रूपी फल प्रदान करते हैं।
यदि समुचित रूपेण अवबोध किया जाये तो कर्म का नियम असीम आशा की वृष्टि करने वाला है। इसके अनुसार मनुष्य का प्रारब्ध उसके अपने हाथों में ही है। उसका भविष्य उसके अपने कन्धों पर निर्भर है। आगामी अनुभवों का स्वरूप उसे स्वयं ही निश्चित करना है। उसे पाप कर्म करने के लिए कोई भी शक्ति विवश नहीं कर सकती। उसे ध्यान रखना है कि वह कैसे व्यवहार करता है, कैसे कर्म करता है और कैसे विचारों का चिन्तन करता है? वह अपने प्रारब्ध का स्वामी है। स्वयं भाग्य-निर्माता है। अपने ही पाप कर्म एवं विचारों के अतिरिक्त उसे इस संसार में अन्य किसी पदार्थ से भी किसी प्रकार का भय नहीं है। उसे यह कहना ही है-"अवांछित अनुभव प्रदान करने की किसमें शक्ति है? इस पृथ्वी पर किसी में भी शक्ति नहीं जो मेरा अनिष्ट कर सके, दुःखी कर सके, अथवा मुझ पर विनाश एवं बुराई की दृष्टि कर सके।" इस प्रकार मनुष्य में अनन्त शक्ति का संचार होता है। आनन्द और ज्योति से पूर्ण भविष्य का निर्माण करने के लिए अपने जीवन का वह स्वयं पथ-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाता है। कर्म का विधान उसे उचित बीजारोपण करने को तथा कर्मों को आदर्श रीति से करने के लिए प्रेरित करता है।
ब्रह्माण्ड के नैतिक स्तर का आधार यही विधान है। इसके अभाव में पाप कर्म को त्यागने और पुण्य कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा न होती। कर्म की यह दोनों विधियाँ इसी महान् नियम से उत्पन्न होती हैं। मनुष्य जानता है कि बुराई की उपेक्षा न करने पर वह अपने लिए घास-पात और काँटे बोता है। उसे विदित है कि उसे अच्छाई करनी चाहिए; क्योंकि परिणामस्वरूप वही अपने अच्छे कर्मों का भाग्यशाली भोक्ता होगा। इस विचारधारा के अनुसार, कर्म का सिद्धान्त भाग्यवाद नहीं है। इसके विपरीत, यह सम्पूर्ण विश्व में नैतिक व्यवस्था के आधार रूप में उच्च सद्व्यवहार का सिद्धान्त है और सिद्धान्त के द्वारा मनुष्य में धीर-धीरे अभय का भाव प्रवेश करने लगता है। यह मनुष्य को अभय तथा अनन्त शक्ति से परिपूर्ण करता है और मन तथा कर्म से आदर्श, भद्र तथा उच्च बनने की तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न करता है। एवंविध, मनुष्य को निर्माता कहा गया है जिसके हाथों में ही सब पदार्थ हैं जिनसे वह इच्छानुसार अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है।
कर्म-पाश से मुक्ति
अन्ततोगत्वा, कर्म का सिद्धान्त यह उपलक्षित करता है कि जीवन के सर्व सम्पन्न पुण्य कर्मों के फलस्वरूप आत्मज्ञान का वरदान प्राप्त कर लेने पर्यन्त मनुष्य जीवन में सुकृत्यों द्वारा अपनी प्रकृति को अधिकाधिक उच्च बना कर तथा पुनर्जन्म प्रदान करने वाले सब कर्मों के ज्ञानपूर्वक त्याग द्वारा जन्म-मृत्यु के पाश से मुक्त होता है और एक बार यह ज्ञान प्राप्त कर लेने पर कर्म का सिद्धान्त निष्क्रिय हो जाता है। बन्धन टूट जाता है। क्यों? सिद्धान्त की क्रिया में गहन ध्यान के उपरान्त हिन्दुओं को ज्ञान हुआ कि यह आत्मा के क्षेत्र में अकार्य-साधक अथवा अक्रियाशील है। केवल शरीर और मन के क्षेत्र में ही यह नियम क्रियाशील है।
जब तक मनुष्य स्वयं को मन और देह का प्रतिरूप मानता है, तब तक वह कर्म-सिद्धान्त के न्यायानुसार इस चक्र में फँसा रहता है। जिस क्षण मनुष्य इस मोह-बन्धन का त्याग कर देता है और इस शरीर-मन की मिथ्या समानरूपता से अनासक्त होता है, तत्क्षण ही उसके अज्ञान का सर्वथा विनाश हो जाता है और शुद्ध चैतन्य के साथ वह अपनी एकरूपता और सर्वातिशयिता का साक्षात्कार करता है। आत्मा को यह ज्ञान हो जाने पर कि वह शरीर और मन से परे है और शुद्ध चेतन स्वरूप है, कर्म का सिद्धान्त उसे स्पर्श नहीं कर सकता। कर्म-चक्र को रोकने की यही विधि है।
स्पष्ट करने योग्य एक और बात यह भी है कि यह सिद्धान्त न केवल बाह्य कर्मों से प्रत्युत मानसिक कर्मों से भी सम्बद्ध है, क्योंकि प्रत्येक कर्म का मूल विचार ही है। इस प्रकार प्रत्येक निश्चित विचार, वह किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसे साक्षात् क्रिया रूप प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं, उसकी गणना मनुष्य के कर्म के अन्तर्गत ही होती है। इसका ज्ञान आवश्यक है। गीता में कर्म की अत्यन्त स्पष्ट व्याख्या आती है कि जब तक मनुष्य अहं भाव से पूर्ण व्यक्ति के रूप में कर्मरत रहता है, तब तक वह शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है। यह क्रमिक प्रगति है। इसलिए हम कहते हैं कि यह विद्यालय गमन की भाँति है जिसमें हम ज्ञानक्रम की समाप्ति पर्यन्त एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश करते रहते हैं और उसी विद्यालय से स्नातक हो जाते हैं। अन्ततोगत्वा, मनुष्य को पूर्णत्व प्राप्त करना है और तभी वह अपने कर्म-नियम से स्वतन्त्र हो कर मोक्ष प्राप्त करेगा। जब तक वह अवस्था प्राप्त नहीं होती, जब तक वह पूर्ण ब्रह्म को अपने कर्म समर्पित करना और शुद्ध नैतिकता ग्रहण करना नहीं सीख लेता, तब तक वह पुनः पुनः शरीर धारण करता रहेगा।
कर्म का विधान और ईश्वर का न्याय
इस विधान के लौकिक स्वरूप और व्यक्तिगत अनुष्ठान के प्रति दो-तीन प्रश्न हैं। एक तो है-इस धरती पर ईश्वर और अनुभवों तथा व्यक्ति के कर्मों के मध्य क्या सम्बन्ध है? हमने कहा है कि ईश्वर व्यक्ति के अनुभवों की सृष्टि नहीं करता, प्रत्युत उसके अनुभव उसके द्वारा उपलब्ध प्रकृति-विशेष के फलस्वरूप निश्चित होते हैं।
अब धरातल पर वर्षा द्वारा सब प्रकार का जीवन प्राप्त होता है; अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वर्षा ही जीवन का कारण है। ऐसा भी होता है कि सार्वभौमिक तत्त्व के रूप में जब वृष्टि होती है और वनस्पति को जीवन-दान प्राप्त होता है। जो जीवन अंकुरित होते हैं, वे सब एक ही प्रकार के नहीं हैं। गेहूँ गेहूँ के रूप में अंकुरित होता है, अन्न अन्न के रूप में और घास घास के रूप में बाहर आती है। वर्षा का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक बीज के भीतर एक अधिकृत प्रकृति निहित है जो पौधों में भिन्न-भिन्न स्वरूप को जन्म देती है, यद्यपि वर्षा समान है और समस्त धरणि पर वह निष्पक्ष भाव से वृष्टि करती है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर यह बीज (संस्कार) है जो मनुष्यों के विचारों में निहित है और वह कर्मों को प्रेरित करता है जिससे मनुष्य के भावी अनुभवों का निर्णय होता है। मन के अनुरूप ही जन्म के समय मनुष्य की प्रकृति का निर्णय होता है और स्वभाव के अनुसार जीवन में नव संस्कार प्राप्त किये जाते हैं।
द्वितीय प्रश्न, जिसका उत्तर मैं देना चाहूँगा वह है-क्या विधान के अन्तर्गत न्याय है? यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छे कर्म करने वाला सुखी नहीं है और बुरे कर्म करने वाला अत्यन्त सम्पन्न है; किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य जिस प्रकार का जीवन यापन कर रहा है और अनुभव प्राप्त कर रहा है, उनका परस्पर हेतुक सम्बन्ध हो। कारण से कार्य तत्काल ही उत्पन्न नहीं होता। वर्तमान में व्यक्ति जिस कर्म में रत है, उन्हें बोये जा रहे बीज माना जा सकता है और उसके अनुभव पूर्व-जन्म का परिणाम हो सकते हैं, विरोध प्रतीत होता है; किन्तु वस्तुतः विरोध नहीं है। एक सहृदय और धार्मिक मनुष्य किसी भागते हुए अपराधी को आपत्ति में सहायता और आश्वय प्रदान करे और भागते हुए अपराधी को आश्रय देने के अपराध में वह स्वयं पकड़ा जा सकता है और उसके स्वयं को अनभिज्ञ कहते हुए विरोध प्रकट करने पर भी उसे फाँसी का दण्ड हो सकता है।
अविचारपूर्वक लोग इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि यह मनुष्य जिसने एक सच्चे ईसाई की भाँति व्यवहार किया और दयावश एक अपने साथ के मनुष्य को विपत्ति में आश्रय दिया, अपना दान का परिणाम भोग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अपराधी को आश्रय देने के फलस्वरूप उसे मृत्युदण्ड मिला। वस्तुतः पुलिस आपको बतायेगी, न्यायाधीश अथवा मृत्युदण्ड से ही आपको ज्ञात होगा कि इस मनुष्य ने एक अपराधी को आश्रय दिया; इसलिए उसको दण्ड दिया गया। किन्तु यदि हम भूमिका पर दृष्टिपात करें तो ज्ञान होगा कि कर्म और उसके अनुभव की सन्निधि मात्र दिखावा है, वास्तविकता नहीं है। दया और सहानुभूतिपूर्ण कर्म भविष्य में श्रेय से पुरस्कृत होगा और मृत्युदण्ड तो भूतकाल के किसी कर्म का प्रतिफल है। नियम अत्यन्त रहस्यमय है और हम इसकी सब क्रियाएँ तत्काल ही नहीं समझ सकते। इसकी सरलतम व्याख्या यह है-"जैसा बोओगे, वैसा पाओगे।" प्रत्येक कारण क्रिया का रूप लेता है; प्रत्येक क्रिया की तदनुरूप प्रतिक्रिया होती है। यह नियम सार्वभौमिक है। यह नियम सर्व व्यक्तिगत अनुभवों में क्रियाशील होता है। अतएव इस नियम के प्रति अत्यन्त जागरूकता से रहो और सत्पथ पर चलो। सुपथ पर चलो। आदर्श जीवन व्यतीत करो और अपना भविष्य शान्त एवं आनन्दमय बनाओ ।
११. रहस्यमय मन और उसका नियन्त्रण
ज्योतिर्मय अमर आत्मन्! मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों और अन्वेषणों के सम्बन्ध में निकट भूतकाल में बहुत-कुछ लिखा गया है; अतएव आज हम जिस विषय का निरूपण करेंगे, उसके अधिकांश भाग से आप पूर्वतः ही परिचित होंगे। पुनरपि मन के सम्बन्ध में विषय इतना महत्त्वपूर्ण और अमूल्य है कि इसकी बारम्बार पुनरुक्ति अनिवार्य है। ये ऐसे तत्त्व हैं जिनका एक बार नहीं, बार-बार ध्यानपूर्वक विवेचन और समीकरण करना चाहिए। यदि ये विस्मृत भी हो जायें, तो पुनः पुनः चिन्तन द्वारा इन्हें स्मरण करना चाहिए। रहस्यपूर्ण मन का ज्ञान पुरातन है। सभ्यता के उदय से ले कर अब तक महापुरुषों ने इन सत्यों का उन्मीलन किया गया है। अनादिकाल से तत्त्वज्ञानी ऋषियों तथा आत्म-साक्षात्कार की ज्योति से प्रकाशित मुनियों ने उन्मीलन द्वारा मनुष्य को उसकी वास्तविक परा-मानसिक प्रकृति का ज्ञान कराया है।
हम कतिपय विशेष पक्षों का निरूपण करेंगे जो इतने नवीन हैं कि कदाचित् अब तक कोई आधुनिक मनोवैज्ञानिक उसके प्रति जागरूक हुआ हो। पश्चिम में मानव-मन का ज्ञान 'वैज्ञानिक ढंग' से प्राप्त किया जाता है। न्यूनाधिक आनुमानिक पहुँच है। शिक्षार्थियों ने व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन प्रारम्भ किया और उनके व्यवहार से, मन से सम्बन्धित कुछ तथ्यों का अनुमान लगाया और तत्पश्चात् उनका जातिशः वर्गीकरण किया। वे मानो 'बाहर से भीतर' की ओर प्रवृत्त हुए। पूर्व में अन्वेषण सर्वथा भिन्न विषय पर हो रहे हैं। उनकी विधि अन्तर्ज्ञान की विधि रही है, उनकी पहुँच 'भीतर से बाहर' प्रवृत्त हुई है। प्रकृति से उनकी विधि अनुमानिक होते हुए भी समय की कसौटी पर निर्दोष सिद्ध हुई; क्योंकि अन्तर्ज्ञान पर आधारित होने के कारण उनका प्रथम प्रक्रम (पूर्वकथन) अमोघ था।
उत्कृष्ट स्थल से मन का निरूपण
पूर्व के आत्म-वैज्ञानिकों ने योगक्रियाओं द्वारा मन से ऊपर उठ कर स्वयं को मन से तथा उसकी गतिविधियों से सर्वथा पृथक् करके, उस श्रेष्ठ स्थल से जो मन से अस्पृष्ट तथा इसके विचारशील स्वभाव से अप्रभावित और सर्वथा मुक्त है, सहनशीलता से इसकी मूलभूत स्वाभाविक प्रकृति और व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने इसका निरीक्षण स्पर्शनीय उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव के प्रकाश में किया जिस पर वे अधिष्ठित थे और जहाँ मन, दर्शनीय और अध्ययन के योग्य द्रष्टा से पृथक् विषय प्रतीत होता था। गत एक-दो शताब्दियों में कितने अर्वाचीन मनोवैज्ञानिक इस प्रकार मन से ऊपर उठ कर इसके अनियन्त्रित प्रभाव से परे जा कर इसके आत्म-स्थल, साक्षी और द्रष्टा बन कर इसकी प्रकृति का अध्ययन करने का दावा करते हैं? महान् योगियों, वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से मनुष्य के अन्तस्तम भाग से परा-मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्त की और मानो वे मन को अपने समक्ष रखने में समर्थ हो गये और अधिष्ठाता एवं विषयाश्रित ढंग से इसकी गतिविधियों का अध्ययन करने में संलग्न रहे।
अपने विषय के अध्ययन में जब निरीक्षक स्वयं ही प्रवृत्त हो, तो उसके परिणाम अपूर्ण और भ्रान्त होते हैं; क्योंकि जिस विषय का वह अध्ययन करना चाहता है, उसमें वह स्वयं भी एक तत्त्व बन जाता है। जब तक उसे पूर्ण रूप से विषयाश्रित ढंग से अध्ययन करना नहीं आता, तब तक विषय की पूर्णतया निर्दोष एवं विशिष्ट विचारधारा प्राप्त करना असम्भव है। यावत्पर्यन्त आपने मन से व्यतिरिक्त किसी शक्ति का विकास नहीं किया (यहाँ पर परा-मानसिक शक्ति का विकास) और आपने निजात्मा को मन से विशिष्ट नहीं किया, तावत्पर्यन्त आप मन के स्तर में स्पर्धापूर्ण अन्वेषण करने में असमर्थ रहेंगे। जैसा कि भारतीय उक्ति है-"आप अपने नेत्रों का दर्शन नहीं कर सकते।" इसके लिए चेहरे के समक्ष दर्पण रखना अनिवार्य है। एवंविध, मन के अध्ययन हेतु मन की कर्मविषयता अपेक्षित है। दीर्घकाल पूर्व महान् ऋषि परा-मानसिक अवस्था को पहुँचने में समर्थ हो गये जिसमें इस प्रकार की कर्मविषयता की समुचित विधियों का प्रयोग किया जा सकता था और उनके गहन अध्ययन से महान् अन्वेषण प्रकाश में आये जिन्होंने मनुष्य को शक्तियाँ प्रदान की हैं, अन्यथा उपलब्धि असम्भव थी।
मन विलक्षण है
पत्थर, वृक्ष, ग्रास और रेत जो शताब्दियों से प्रदत्त भौगोलिक क्षेत्र में सत्तारूढ़ हैं, अपने भौतिक वातावरण के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं रख सकते; किन्तु एक मेधावी पुरुष उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनसे सम्बद्ध असंख्य तत्त्व एकत्र कर लेता है। वह इन तत्त्वों का इतरेतर सम्बन्ध खोजता है और इस प्रकार एक उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उदाहरणतः वह मृत्तिका की रचना और खनिजों का योग, भूमि से उसका सम्बन्ध, सूर्योदय, जलप्रवाह और वायुवेग की दिशाओं का ज्ञान निश्चित कर सकता है। पत्थर और चट्टानें अचल और जड़ हैं। तृणादि, अपने तथा परिसर के प्रति सर्वथा अचेतन हैं। जिस भूमि में वे उत्पन्न होते हैं, उसका भी उन्हें ज्ञान नहीं। उस पर चल रही बायु अथवा अभिषिक्त जल के प्रति वे अनभिज्ञ हैं। अद्भुत तत्त्व है जो उसे अपने परिसर के सम्बन्ध में तत्काल बोध प्रदान करता है और इसके साथ ही उसे ज्ञानसंवर्धन की योग्यता प्रदान करता है जिसमें से उसके लिए विचारों का उद्भव होता है। यह क्रिया मानव-जीवन का रहस्य है। यह मन का रहस्य है।
यदि आप इस आश्चर्यान्वित मानसिक शक्ति से युक्त हैं तो आप जहाँ पर जायें ज्ञान के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं, जब कि इस शक्ति के अभाव में आप मात्र कंकड़, पाषाण अथवा शाक (बन्दगोभी) के समान हैं। सुप्तावस्था में मन के निद्रालीन होते ही आप सब व्यावहारिक ज्ञान खो बैठते हैं। जिस क्षण मन संहरण करता है, उसे आपको छोड़ कर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तत्क्षण आप पाषाणवत् हो जाते हैं। आप जब भी सुप्तावस्था को प्राप्त होंगे, तभी आपकी यही दशा होगी। जीवन से सम्बद्ध मन जब पुनः क्रियाशील होता है, तब जीवन से सम्बद्ध सम्पूर्ण अद्भुत गति नवीन रूप से प्रारम्भ होती है।
'मन' नाम की यह कौन-सी वस्तु विशेष है जिसकी क्रियाशीलता मनुष्य को सृष्टि का स्वामी बना देती है और जिसकी निश्चलता उसे निर्थरक और सत्ताहीन बना देती है? यह कौन-सा रहस्यमय पदार्थ है जिसकी गति एवं निश्चलता से तथा विस्तरण एवं संहरण से हमारे व्यक्तित्व में इतने भेद का आभास होता है? पाँच मिनट में मनुष्य समस्त दृष्टि और अवेक्षणा को सूचनाओं के सुव्यवस्थित तथ्यों में परिणत कर सकता है और चिच्छक्ति तथा सम्पदीकरण की प्रक्रिया द्वारा वह इन्हें ज्ञान के अवबोधपरक क्रम में संयुक्त करता है। मन के विचारों द्वारा प्रेरित मनुष्य चलने और बोलने तथा विविध संश्लिष्ट गतिविधियों को क्रियान्वित करने में समर्थ होता है, यह भी कम अचम्भा नहीं है।
अपने मन के आन्तरिक अचम्भे के प्रति मनुष्य अत्यन्त अचेत और अज्ञात है। विचार को विचार कौन देता है? मन पर मन को प्रेरित करके इसके प्रति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कौन करता है? क्या आपने मन पर स्वाधिकार नहीं मान लिया है? यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो ज्ञात होगा कि विक्षिप्त होने पर आप कितने भयभीत हो उठते हैं। उस गृह में अथवा परिवार में इससे महत्तर और दुर्घटना क्या हो सकती है कि इसके परिवार के किसी सदस्य का मन विक्षिप्त हो जाये? मन के खो जाने पर मनुष्य मनुष्य प्रतीत नहीं होगा। अकस्मात् ही तब आपको बोध होता है कि वास्तव में मन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है जिसके थोड़ा-सा भी विक्षिप्त होने पर जीवन नष्ट-सा हो जाता है। एक सुविख्यात सज्जन पुरुष किसी सन्ध्या को थोड़ा अधिक पी लेता है तो उसकी चिन्तन-प्रक्रिया मद से सम्भ्रान्त हो जाती है और वह अपने अधीन गौरव एवं मित्रों तथा निन्दक दर्शकों के समक्ष स्वयं ही मूर्ख बनता है। नशा लेने वाला मनुष्य जिसका मानसिक सन्तुलन निरुद्ध हो, वह जीवित ही मृत के समान है। मानसिक सन्तुलन बिगड़ने से सम्पूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना मान खो बैठता है जो उसे पूर्व प्राप्त था। वह अपना महत्त्व खो बैठता है-अपना व्यक्तित्व खो बैठता है।
मनुष्य को प्रभु-प्रदत्त मानसिक शक्ति सर्वोच्च उपहार है। इससे बढ़ कर और अधिक अमोघ कोई उपहार नहीं है। मनुष्य का स्वभाव मन से संयुक्त है; किन्तु दुर्भाग्यवश यही मन एक महानतम अभिशाप भी हो जाता है। यह असत्याभास जीवन के महान् रहस्यों में से एक है। अनुभव से प्रत्येक व्यक्ति को विदित है कि क्षुधावस्था में मन मनुष्य का कितना अनर्थ कर सकता है। तथापि उस प्रक्रिया की प्रकृति, मनुष्य और पशु जाति के मध्य विशेष अन्तर को लक्षित करती है। यह श्रेष्ठतम शक्ति मनुष्य को ईश्वर की सृष्टि में उत्कृष्ट पद प्रदान करती है और पार्थिव सत्ता के इस देहबन्ध में जीवन में यह अपरित्याज्य है।
हम देखते हैं कि सुख और दुःख सर्वथा मन की अवस्था ही है। आसक्ति, अनन्त इच्छाएँ तथा असंयत आवेग व्यक्ति का पतन कर देते हैं। वे मानसिक अवस्था को निम्न करते हैं। अशान्ति, घोर संक्षोभ एवं गम्भीर व्याकुलता इसके परिणाम हैं। इन सबका अनुभव पीड़ा, दुःख और क्लेश के रूप में होता है। परमात्मा ने और कितने भी लाभ प्रदान क्यों न किये हों, ये मनो-अनुभूतियाँ मनुष्य को शोकग्रस्त करती हैं। आपका परिवार हो, मित्र हों एवं अन्य समृद्धि भी हो; किन्तु यदि मन अनियन्त्रित कामनाओं से असन्तुलित अथवा अव्यवस्थित हो गया है, तो इहलोक में परमात्मा की दी हुई सर्वोत्तम वस्तुओं को भी वह नरक का द्वार बना सकता है। अतएव मन का अवबोध करने तथा इसका समुचित उपयोग करने के पीछे एक महान् उद्देश्य निहित है। मन एक साधन के समान है। विचार आपके पास सर्वोत्कृष्ट शक्ति है। सबने यह श्रवण किया है; किन्तु वस्तुतः शक्ति क्या है? और 'विचार की शक्ति है' का वास्तव में अभिप्राय क्या है? विचार स्वयं ही आपकी प्रसन्नता और उदासीनता है। विचार ही आपका बन्धन और मोक्ष है। विचार ही आपका स्वर्ग और नरक है। विचार ही आपको बना सकता है और आपका नाश कर सकता है। जब विचार-प्रक्रिया आत्यन्तिक रूप से शान्त हो जाती है, जीवनान्त हो जाता है। अतः विचार ही जीवन है।
मन और विचार दो पृथक् तत्त्व नहीं हैं। यदि मनुष्य क्षणिक रूप से अथवा सदा के लिए विचार को रोक सकता है, तो उसके लिए मन का अस्तित्व नहीं रहता; किन्तु यदि ऐसा सहज ही हो जाये तो मनुष्य का विनाश हो जाता है; किन्तु यदि ऐसा विचारपूर्वक वैज्ञानिक ढंग से किया जाये तो मनुष्य ब्रह्माण्ड का स्वामी बनता है। बह समस्त विश्व को वश में कर सकता है; क्योंकि स्वर्ग पर उसका प्रभुत्व होता है। मानसिक प्रक्रियाओं का मन के पूर्ण नियन्त्रण द्वारा सम्पूर्ण एवं निःशेष निरोध मनुष्य को तत्काल ही उसके वास्तविक अस्तित्व का बोध कराता है। जब मन का पूर्णतया निराकरण कर दिया जाता है, तब आपके वास्तविक अस्तित्व की अनुभूति आपकी निजी हो जाती है। आप विश्राम लेते हैं और अपने ही सच्चे स्वरूप में वास करते हैं।
मानव-चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में कभी नहीं रहती। इसे मन आवेष्ठित कर लेता है, स्तम्भित कर देता है और प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है और वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य की प्रक्रिया में विघ्न-स्वरूप बन कर आता है। आपको मन की साधन-रूप में अवधारणा करनी चाहिए; क्योंकि इसके स्वभाव और गतिविधियों का बोध होने पर आप इसे प्रभु के वरदान की महानतम शक्ति के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब इसका समुचित ज्ञान नहीं होता, इसके नियन्त्रण के सम्बन्ध में जब किंचिदपि बोध न हो, तब आप मन के हाथों में मात्र एक खिलौना है। स्वयं को मन का स्वामी जानिए, अन्यथा आप स्वयं को विचारक यन्त्र मानने की भूल कर बैठेंगे। आप विचारक यन्त्र नहीं हैं। आप विचारशील हैं। मन रूपी विचारक यन्त्र के स्वतन्त्र अधिष्ठाता और नियन्ता है। इस ज्ञान के अभाव में आप मन के दास बन जाते हैं। मन की स्वच्छन्दता के अनुरूप आप प्रेरित होते हैं। आपको शान्ति प्राप्त नहीं होती। तूफानी जल की सतह पर कार्क (पिधान) के टुकड़े की भाँति मन को प्रयोग करने की अपेक्षा स्वयं ही उसके शिकार बन जाते हैं; आप निःसहाय हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
मानव और ईश्वर के मध्य मन-एक बाधा
यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य और शरीर तथा व्यक्तित्व एवं बाह्य संसार के मध्य मन ही एक श्रृंखला है। शैशवकाल से ही मनुष्य संसार के सम्बन्ध में मन के माध्यम से सर्वज्ञान प्राप्त करता है। इन्द्रियाँ स्वीकृत तत्त्वों से मन को भोजन प्रदान करती हैं। वस्तुतः मन ही उन स्वीकृत तत्त्वों से सम्बन्ध स्थापित करके ज्ञान को जन्म देता है। एवंविध मानव-जीवन का यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग है। इस तत्त्व की महत्ता पूर्व ने विदित की है; किन्तु इससे भी अधिक, पूर्व वालों को मन के सम्बन्ध में कुछ और भी कहना है जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा अकथित है। पूर्व ज्ञान के मतानुसार मनुष्य और उसके सच्चे स्रोत (भगवान्) के मध्य मन एक महत्तम बाधा है। यही बाधा ही उसे अनन्त की अनुभूति नहीं करने देती। मनुष्य एक अव्यापक व्यक्तित्व के परिणाम में संकुचित और सीमित है। चैतन्य के सीमित क्षेत्र से परे जाने और विस्तृत होने के लिए मनुष्य संघर्ष करता है और सीमित मन इसका सर्वदा प्रबल विरोध करता है।
समझाने के लिए मनुष्य के जीवन में संयम और मनोजय (मन-रूपी बाधा का अतिक्रमण) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है। मन पर विजय प्राप्त करनी है। आपको निज सत्ता की परमावस्था के उस चैतन्य का आश्रय प्राप्त है जहाँ कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं है। इस दृष्टिगोचर संसार के क्षणिक अनुभव के पीछे वह निर्विकार सत्ता उसी प्रकार से निहित है जिस प्रकार से चलचित्र में हलचल तथा चलते हुए चित्रों के पीछे अचल चित्रपट जो द्रुतगति से इस पर नाटक दिखाये जाने के उपरान्त भी अन्त में अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार से सब सीमित अनुभवों के पीछे वर्णनातीत शुद्ध सत्ता का अपरिवर्तनशील असीम आधार विद्यमान है। वह अविनाशी है। वह अक्षय अविकारी अवस्था ही आपका सत्य आधार है। वह आपका परम धाम है। वह स्वतन्त्रता (मोक्ष), अभय एवं आनन्द की अवस्था है और मन के बन्धन से वह आपके लिए अवरुद्ध है।
वस्तुतः उस अनुभव की प्राप्ति के लिए मन किस प्रकार इन्कार करता है? यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य आधारित है। मन किस प्रकार अवबोध प्राप्त कर सकता है और इसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है? यह एक प्रश्न है, पश्चिम में जिसकी उपेक्षा की गयी है। अत्यन्त कलापूर्ण ढंग से मन विघ्न-रूप बनता है और मनुष्य की परम सत्ता तक पहुँचने में बाधक बनता है। यह आपसे छिप कर अथवा आपको अनुभव-प्राप्ति से रोक कर घातक कार्य नहीं करता अर्थात् यह वास्तव में परमानुभूति और आपके मध्य अधिष्ठित नहीं होता। वस्तुतः आप उस मन की अपेक्षा उस परम चैतन्य रूप परमात्मा के अधिक निकट हैं। यह परमानुभूति आपके हृदय के अन्तरतम भाग से अभिलक्षित होती है और मन का स्वभाव मनुष्य को बहिर्मुख करना और केन्द्र से सदा दूर रखना है, इस कारण से यह विघ्न स्वरूप है। हृदय के गहनतम भाग में प्रवेश करने से रोकता हुआ यह सर्वदा आपको ऊपरी सतहों में रहने के लिए आकर्षित करता है। इच्छाओं, बहिर्मुखी प्रवृत्तियों और निषेधात्मक प्रकृति के कारण मन आपको अपने केन्द्र से दूर ले जाता है और आपके व्यक्तित्व के बाह्य जगत् के विविध नाम और रूपों में भटकाता है। इस प्रकार से मन गतिशील रहता है। यह आपको अपने सत्य चेतन स्वरूप से विमुख करके बाह्य जगत् में ला फेंकता है।
पाश्चात्य मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव
पाश्चात्य मनोविज्ञान ने मन का निरूपण व्यवहार और क्रिया-विशेष के रूप में किया है। जिस रूप में उनका ध्यान मन की ओर आकर्षित हुआ, उसी पर वह पहुँच आधारित है। मूलतः पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। उन्होंने चिकित्सालयों में कार्य प्रारम्भ किया जहाँ विविध रोगों की चिकित्सा और शोधन-कार्य किया जा रहा था; किन्तु उन्हें विदित हुआ कि कतिपय विशेष रोगों का उपचार औषधीय विज्ञान द्वारा असम्भव था। इस प्रकार से वे इस विषम तथ्य पर पहुँचे कि अनेक रोगों का मूल कारण मस्तिष्क था। इस अन्वेषण से वे मानसिक प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए कार्यरत हुए और ज्ञात किया कि मन और शरीर की क्रियाओं के मध्य कुछ स्पष्ट, विशेष सम्बन्ध थे। प्रारम्भ से ही इन पाश्चात्य विद्वानों के निरीक्षण उन रोगियों तक ही सीमित थे जिन पर औषघ का कोई प्रभाव नहीं होता। एवंविध, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि पश्चिम में मन का अध्ययन विकृत (अस्वस्थ) मनोविज्ञान से प्रारम्भ हुआ। व्याधित मन ही मनोवैज्ञानिकों के ध्यान का केन्द्र था।
उनके निरीक्षणों से एक महान् विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, किन्तु इसकी उन्नति में वैज्ञानिकों को विशेष लाभ न हुआ; क्योंकि वे मन के वास्तविक स्वरूप के अध्ययन से अनभिज्ञ थे। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के मन के निरूपण की अपेक्षा उन्होंने अस्वस्थ मन का निरूपण किया। उन्होंने प्रतिनिधित्व करने वाले मनुष्य का नहीं, वरंच एक विशिष्ट तथा असामान्य व्यष्टि मन का निरीक्षण किया। दूसरी ओर, पूर्व के महान् ऋषियों ने समष्टि मन का अध्ययन किया। मन जीवन का आन्तरिक केन्द्र है और उनके अध्ययन का उद्देश्य इसके सार्वभौम रूप का निरीक्षण था- 'इस दिशा में, 'उस दशा में', स्वस्थ अथवा अस्वस्थ मन का निरीक्षण नहीं था। पूर्वीय विद्वानों ने स्थूल तत्त्व और आत्म-तत्त्व का भी विचार किया और अवधानपूर्वक उनके तथ्यों का परस्पर सम्बना स्थापित किया। उन्होंने अन्तरात्मा में गोता लगाया और अन्तर्दृष्टि तथा ध्यान द्वारा इस अन्तःसाधन मन के अद्भुत तथ्यों का उद्भेदन किया। उनका अध्ययन शुद्धरूपेण विषयीपरक था। ध्यान में पूर्वीय विद्वान् विषय की गहराई तक पहुँचे और वहीं उन्हें सत्य का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। अतः उन्होंने मन के प्रतिज्ञातव्य तथ्यों की उद्घोषणा विश्वास के साथ की है। एवंविध इस सिद्धान्त का पूर्वीय प्रादुर्भाव पाश्चात्य मनोविज्ञान से सर्वथा भिन्न था।
मन की विशेषताएँ
मन की प्रमुख विशेषता है-विमुखता। ऋषियों ने बताया कि मन की गति बहिर्मुखी है, अन्तःकरण में केन्द्रित नहीं है। यही जीवन का सिद्धान्त है-प्रत्येक वस्तु का विस्तरण केन्द्र से बाहर की ओर होता है। किन्तु एक ऐसी शक्ति है जो सबको अपने स्रोत और केन्द्र की ओर पुनः आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। बहिर्मुखता का अतिक्रमण करने पर अर्थात् अन्तर्मुख होने पर मनुष्य अपनी पुनः एकत्रित अखण्ड शक्ति का निस्तार करने में सक्षम हो जाता है और इस प्रकार से अपने स्रोत को पा लेता है। इतना होने के पश्चात् उसकी खोज समाप्त हो जाती है। जीवन पर प्रभुत्व हो जाता है।
मन की दूसरी विशेषता है-अनवरत कर्मशीलता। क्षण-भर के लिए भी मन निष्क्रिय नहीं होता।
तीसरी विशेषता है-कर्मक्षेत्र में विस्तार। यह न केवल एक दिशा, प्रत्युत अनेक दिशाओं में क्रियाशील है। अभी यहाँ है, अब वहाँ है और अब सर्वत्र है।
इस प्रकार बहिर्मुख, सतत क्रियाशील और एक विषय से दूसरे की ओर उड़ते हुए मन का नियन्त्रण अत्यन्त दुष्कर है। इसे समझने के लिए पर्याप्त सूक्ष्मता की आवश्यकता है। यह चक्षुर्विषय नहीं है; परीक्षण-नलिका में डाल कर इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है; सूक्ष्मदर्शन-यन्त्र से इसे देखा नहीं जा सकता। यद्यपि मनुष्य का मन पर कदाचित् ही आधिपत्य है, तथापि मन मनुष्य से सर्वस्व करा सकता है। यह इतना सूक्ष्म, आन्वीक्षिक पूर्णतः अन्तस्थ है कि इसे ग्रहण करना अत्यन्त कठिन है। एक क्षण तो यह प्रशान्त महासागर अथवा बाह्य अन्तरिक्ष के विचार में विस्तृत हो सकता है और दूसरे क्षण सरसों के बीज अथवा सुई की नोंक अथवा अणु के विचार के समान सूक्ष्मकाय हो सकता है मानो यह असीम पर्यन्त सब पदार्थों का चिन्तन कर सकता हो। एक ही छलाँग में यह समस्त नक्षत्र, चन्द्र और सौर-मण्डल को पार कर सकता है और उसी क्षमता से यह रेत के कण के समान लघु पदार्थ का चिन्तन कर सकता है, कितना रहस्यपूर्ण है मन!
प्रत्येक मनुष्य में मन तीन आवर्तक अवस्थाओं अथवा दशाओं को प्राप्त करता है। इन्हीं तीन अवस्थाओं में से चैतन्य किसी एक के द्वारा प्रक्रिया करता है (जिसे वेदान्त-दर्शन में 'अवस्था' कहते हैं)। यह बाह्य अथवा अन्तः हो सकती है और यदि यह आभ्यन्तर है, तो अंशतः अथवा पूर्णतः इसका संहरण हो सकता है। जितना समय मन बाहर की ओर प्रवृत्त रहता है, उसे 'जागृतावस्था' कहते हैं। रात्रि में जब आप निद्रा के लिए जाते हैं, तब मन बाह्य लोक से अंशतः अपाकृष्ट हो जाता है; किन्तु भीतर से पुनरपि प्रबल रूप से क्रियाशील होता है। इसे आप प्रायः 'स्वप्नावस्था' कहते हैं। इसमें मन एक सृष्टि का सृजन करता है, अनुभव पूर्वाख्यात 'जागृतावस्था' में प्राप्त अनुभवों के समान होता है।
मन जब इस स्वप्न-बोध से परे जाता है, यह और अधिक गहराई में डूब जाता है और पूर्णतः संहत और लीन हो जाता है। यह तृतीयावस्था जिसकी अनुभूति आप प्रतिदिन करते हैं, 'गाढ़ निद्रा' कहलाती है। इस अवस्था के प्रति आपको अल्पज्ञान रहता है और कदाचित् ही आप इसका चिन्तन कर सकते हैं; किन्तु वस्तुतः यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसी में आपके अन्तस्तम अन्तःकरण में अधिष्ठित 'आत्मा' की कुंजिका निहित है। मन की पूर्ण संहृत इस गहन, स्वप्न रहित गहन निद्रा की इस अवस्था में आप अपनी सत्य, शाश्वत आन्तरिक प्रकृति के निकट पहुँचते हैं। इस अवस्था में मन अपने स्रोत और केन्द्र के समीपस्थ होता है; किन्तु साथ ही वह पूर्णतः विलुप्त भी रहता है और इसके अन्तस्तम और मूल 'अहं' विचार की प्रक्रिया निरुद्ध हो जाती है। इसकी विद्यमानता का शून्यप्राय लक्षण असन्दिग्ध अहंभाव है जो मनुष्य के जागृतावस्था में आने पर इतना ही होता है-"मैं गाढ़ निद्रा में सोया", "मैंने खूब विश्राम किया।"
मौलिक विचार
मन अपने केन्द्र में ही स्थित क्यों नहीं रहता है? पुनः बाह्य चेतना में आने के लिए इसे कौन प्रेरित करता है? प्रथम उत्तर तो यह है कि स्वभावतः ही मन बाहा प्रवृत होता है। द्वितीयतः 'अहं-भाव' का अनियन्त्रित संवेग इसे स्वकेन्द्र में स्थिर रहने से रोकता है। यह मौलिक विचार 'अहं' आपके सीमित, मिथ्या, पृथक् व्यक्तिगत अस्तित्व का आधार है और यह मौलिक विचार है जो रहस्यपूर्ण ढंग से आपको शरीर, इन्द्रियाँ, मन और इसके भाव तथा नाम और रूप से सायुज्य प्राप्त करने की भ्रान्ति में प्रवृत्त करता है।
मन के ग्राह्य इस मौलिक स्वरूप की प्रकृति क्या है? यह सार्वभौमिक नामकर्ता है. और सर्व सामान्य व्यक्तित्व की आधार रूप प्रकृति है। इस धरातल पर प्रत्येक व्यक्ति के मन की भूल यही है। इसे अँगरेजी भाषा में सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसका स्वरूप सर्वभाषाओं में दृष्टिगोचर है। आध्यात्मिक रूप से यह आन्तरिक उद्भेद का मुख्य शत्रु है। मन के सभी विभ्रम इसी से उत्पन्न होते हैं। यह अहं-विचार है। यह विचार आपके मन में प्रतिदिन अनेक बार उठता होगा। जागृति में आपके मन में उठने वाला प्रथम विचार यही होता है। घोर रात्रि में गहन निद्रा से अकस्मात् जागने की कल्पना करें-नेत्र-उन्मीलन से पूर्व ही आपमें प्रथम विचार 'मैं' का ही उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् यह 'अहं' आपके समक्ष सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को उपस्थित करता है। आपको आभास होता है कि यह मध्य रात्रि है और आप धरणी से ढाई फुट ऊपर एक शय्या पर शयन कर रहे हैं। समय और अन्तरिक्ष, जो ब्रह्माण्ड के प्रमुख तत्त्व हैं, इसी 'अहं' के विचार से ही उद्भूत होते हैं। इतना होने पर रहस्यपूर्ण ढंग से आपको सायुज्य प्राप्त होता है। आप जानते हैं, आप कौन हैं-आपका नाम, आपकी आयु, आपका मिथ्या सीमित व्यक्तित्व ! यह मन का विनाशक कार्य है। आपके मनोवैज्ञानिक अस्तित्व का मूल आधार अहं भाव सर्वप्रथम उदित होता है और तदुपरान्त सदेह व्यक्ति का समस्त आकार इसके ऊपर आलम्बित किया जाता है।
इस आकृति से विचार उत्पन्न होता है- 'मेरा' । शय्या पर पड़े हुए ही आप अनुभव करने लगते हैं-"मेरा पृष्ठ भाग संहत है", "मेरे पाँव शीतल हो रहे हैं", "मेरा कण्ठ अवरुद्ध है", "शीत है।" अब आपको विश्राम और उष्णता चाहिए। आपको इसकी इच्छा हो अथवा नहीं "मैं" और "मेरा" से मूल स्वार्थ जागृत होता है। नैतिक अथवा आध्यात्मिक रूप से इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यह 'स्वार्थपरता' मन की प्रक्रिया का स्वाभाविक उद्भाव है और सामान्य व्यक्ति की मूल प्रकृति है। प्रत्येक को अपने लिए किसी-न-किसी पदार्थ की आवश्यकता है। यह इतना ही पुरातन तथ्य है जितना यह संसार और मानव-समाज इसी मूल तथ्य पर कार्यरत है, यद्यपि यह तथ्य अप्रिय क्यों न हो। आप कह सकते हैं- "मैं निःस्वार्थी हूँ"; किन्तु निहित सत्य यह है कि आप निःस्वार्थ होने का नाटक करते हैं; क्योंकि अमुक व्यक्ति से आपको कुछ अभिप्राय है। उससे आपको कुछ प्राप्ति होती है जो आपको प्रिय है और आपको प्रफुल्लित करती है। मनुष्य के प्रत्येक कर्म के पीछे निःस्वार्थता में भी एक गूढ़ अन्तः उद्देश्य निहित होता है। इस उद्देश्य में, इस स्वार्थता में जीवन का केन्द्र, व्यक्तित्व का केन्द्र निहित होता है। एवंविध मानव-सत्ता का सूक्ष्म आधार स्वार्थ है।
कर्म में सर्वदा भ्रमित मन के चक्र के मानो दो आरे हैं। ये दो आरे आकर्षण और अपकर्षण, इच्छा और अनिच्छा हैं। वह क्या वस्तु है जो मनुष्य को रुचिकर है? उसे वे पदार्थ रुचिकर हैं जो सुखद, विश्वामप्रद और सुविधापूर्ण हों। दुःखद, श्रान्तकर और अप्रिय पदार्थ उसे रुचिकर नहीं हैं। इस चक्र का केन्द्र अहं-भाव है।
जैसे ही यह विपरिवर्तमान चक्र अहं पर सहसा प्रकाशित होता है और इन्द्रियाँ रुचिकर तथा अरुचिकर पदार्थों के प्रतिबिम्ब ग्रहण करती हैं, मन में इच्छाओं का प्रादुर्भाव होता है, सम्पर्क प्राप्त करके प्रिय और रुचिकर पदार्थों की प्राप्ति तथा अप्रिय तथा अरुचिकर पदार्थों की उपेक्षा की कामनाएँ जागृत होती हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन का विश्लेषण करने पर आपको जीवन के समस्त कार्यकलापों को चलाने वाली दो ही प्रकार की क्रियाओं का ज्ञान होगा; क्योंकि सभी क्रियाएँ या तो अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति हेतु संघर्ष में घटित होती हैं या अवांछित पदार्थ के परिहार हेतु कार्यान्वित होती हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा यदि इस प्रकार के प्रयास में विघ्न अथवा प्रतिरोध आ जाये तो क्रोध की अनुभूति होती है। इच्छा के जागृत होने पर उसकी पूर्ति न हो तो घोर विश्रान्ति और उत्तेजना प्रस्फुटित होती है। तदुपरान्त, इच्छा के अनुभव पर उसकी जब पूर्ति हो जाती है; किन्तु प्रत्याशित विचारधारा के किंचिद् विपरीत होती है, तब क्या होता है? तब निराशा होती है, दुःखद विभ्रम होता है और इच्छा के पूर्णरूपेण प्रत्याशित रूप से पूर्ण हो जाने पर मन में उस पदार्थ अथवा प्राप्त अनुभव-रक्षण की चिन्ता-सी जागृत होती है कि यह कहीं शीघ्र ही समाप्त न हो जाये क्योंकि इसका अन्त होना है और होता है; क्योंकि सब पदार्थ ससीम हैं और इसीलिए अचिरेण परिवर्तन, विनाश एवं क्षय को प्राप्त होते हैं। इससे भी बुरा और क्या होता है? यदि व्यक्ति को किसी विषय की प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो एवं वह अन्य व्यक्ति को पूर्वतः ही उसका सुख लेते हुए देखता है तो ईर्ष्या, घृणा और द्वेष के भाव उसे सताने लगते हैं और वह मानसिक शान्ति खो बैठता है।
यह सब भाव मूल विचार- 'मैं' और इसके प्रमुख उत्तराधिकारी 'मेरा' से उत्पन्न होते हैं। वे सब एक-दूसरे का अविश्वास गति से अनुगमन करते हैं कि मनुष्य का समस्त जीवन अनवरत रूप से इस रहस्यपूर्ण वस्तु 'मन' के सदा गतिशील, परिवर्तनशील भावों, विचारों और संकल्पों की आन्तरिक झनझनाहट से भरा रहता है। 'मैं' और 'मेरा', रुचि, अरुचि, इच्छा, व्याकुलता और फिर क्रोध, निराशा, स्वार्थपूर्ण वर्ष (स्वाभिमान), आसक्ति, ईर्ष्या और घृणा मन को सदा दुःखी करते हैं और इसे शोक (उत्ताप) में रखते हैं। यह सामान्य गति है मन जिसका अनुसरण करता है। क्यों? क्योंकि मन ने अपने से बाहर के पदार्थ-चिन्तन में निज-अस्तित्व को खो दिया है। स्वभावतः, बाहर जा कर यह बाह्य पदार्थों से आसक्त और परिबद्ध हो कर असंख्य बाह्य प्रक्रियाओं में प्रवृत्त हो जाता है। भीषण आसक्ति और बन्धन ही अति-विवेकशील मन का प्रारब्ध है और सामान्य मनुष्य का विवेक अन्धकारमय हो जाता है। इसके पश्चात् जो होता है, वह अधिक अर्थपूर्ण है। जिस क्षण मन इन्द्रियों के सम्पर्क द्वारा इच्छित पदार्थ का संस्कार प्राप्त करता है, एक अत्यन्त सार्थक घटना घटित होती है जो आपको निज मन के अन्य चकित करने वाले पक्ष का अध्ययन करने को बाध्य करती है जो वस्तुतः महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इसमें मन इन्द्रियों तथा बाह्य पदार्थों के सम्पर्क से प्राप्त अनुभव को तत्काल अंकित कर लेता है। मन में एक सूक्ष्म आन्तरिक संस्कार बन जाता है। यह संस्कार प्रायः आलोप्य होता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता।
सूक्ष्म संस्कारों की प्रक्रिया
जिस प्रकार माटी में बीज बोया जाता है, उसी प्रकार से प्रत्येक अनुभव का संस्कार मन के ऊपर बन जाता है। अनुभवों के यह संस्कार 'जीवित' होते हैं। प्रथमतः जिन कारणों से इन संस्कारों का जन्म हुआ, उन अनुभवों को पुनः जागृत करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। वस्तुतः मन प्रत्येक संस्कार के अनुरूप वास्तविक अनुभव को पुनः जागृत करने की प्रवृत्ति रखता है।
पूर्ण किये जाने पर इच्छा को सदा बल प्राप्त होता है। यह इच्छा का स्वभाव ही है। इस प्रकार जैसे एक अनुभव-विशेष का संस्कार अथवा इच्छा-पूर्ति का संस्कार उसी इच्छा की क्रमिक पूर्ति द्वारा अधिकाधिक निश्चयेन दृढ़ हो जाता है, वह संस्कार मन में सुनिश्चित भाव बन कर परिपक्व होने लगता है। पूर्ति द्वारा इच्छा कभी सन्तुष्ट नहीं की जा सकती। मन की वृत्तियाँ तो मानो उत्तेजना की प्रतीक्षा में रहती हैं जैसे ही इच्छित पदार्थ पुनः बाहर दृष्टि में आता है अथवा उसके प्रति श्रवण अथवा चिन्तन किया जाता है तत्काल ही इच्छा जागृत होती है। यह अभिव्यक्त होती है और मन को बाहर जाने के लिए उत्तेजित करती है। जब ये विचार की लहरें मन में प्रवाहित होती है तो कल्पना को रंगमंच पर इसे दर्शाने के लिए आमन्त्रित किया जाता है कि इष्ट विषय कितना मधुर और कमनीय है तथा इसके आकर्षण कितने लुभावने हैं। जैसे ही कल्पना इस प्रकार से व्यक्त होती है, यह विचार प्रबल तृष्णा के रूप में अभिव्यक्त हो उठते हैं। कल्पना-बद्ध ऐसे विचार मनुष्य को बन्धन में डालते हैं। मन के विविध भावों के साथ उसका सम्पूर्ण सायुज्य उसे अन्तःकरण में क्रियाशील इच्छाओं का दास बना देता है। इस प्रकार उत्तेजना जागृत होने पर आप उसके द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। अहंकार का इच्छा-पक्ष भी मन की इच्छा प्रकृति के बन्धन में पड़ जाता है। इस प्रकार से सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ही भार वहन करना पड़ता है और व्यक्ति इच्छा-पूर्ति हेतु कर्म में धकेल दिया जाता है, उसे क्रियारत होना पड़ता है। इच्छा-पूर्ति होने पर विशाल चक्र एक बार पुनः पूर्ण हो जाता है। वह अनुभव पुनः प्राप्त कर लिया गया है और मन पर अंकित संस्कार और भी दृढ़ कर दिया जाता है।
यह चक्र है जिसमें मनुष्य फँस जाता है। वह एक खिलौने, कठपुतली अथवा मन की एक खेलने की वस्तु के समान है जो किसी प्रकार का संयम नहीं चाहता। इसके प्रति जागरूक न रहने और इसे आधिपत्य में न रखने पर मनुष्य कठपुतली की भाँति जीवन वास करेगा और दास की भाँति प्राणान्त ! अधिकांश मनुष्य मन की प्रत्येक अल्प इच्छा और उत्तेजना से प्रभावित हो कर अपसृत हो उठते हैं। वे स्वतन्त्र नहीं हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र एक कल्पित-कथा है। निष्कर्ष की स्वतन्त्रता, वाणी की स्वतन्त्रता और चार्ल्स द्वितीय के (१६७९) के हैबियस एक्ट उन्हें प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु यदि उन्होंने अपने मन को संयत नहीं किया, इच्छाओं और वासनाओं को वश में नहीं किया तो वे सभी वस्तुतः दासता में हैं और उनकी स्वतन्त्रता नाम मात्र की है।
मनुष्य को जब मन के क्रियाकलापों का बोध हो जाता है (किस प्रकार 'मैं' ही मन का मूल विचार है) और वह इसकी गति को समझने लगता है तब वह इस पर नियन्त्रण कर सकता है। मन के सम्बन्ध में एक अत्यन्त रोचक तथ्य है-क्योंकि 'मैं' विचार सर्वथा मन के वश में है, मनुष्य अपने अस्तित्व के अन्तस्तम कोण में प्रवेश करने में असमर्थ है जहाँ उसके चैतन्य का वास है। इस पूर्वोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि मन मनुष्य को मोक्ष का अनिर्वचनीय अनुभव कराने से रोकता है।
अब मनोजय कैसे प्राप्त करें
अब समस्या का वर्णन स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। समाधान क्या है? समाधान इस समस्या के सर्वथा प्रतिकूल चलने में है। प्रथमतः, इच्छाओं को वश में करके मन की बहिर्मुखता को संयत करने का प्रयास करना चाहिए। कहना तो अत्यन्त सरल है; किन्तु इच्छाओं का अतिक्रमण कैसे हो? यह इतना सरल नहीं है। सम्यक् विचार और विवेकशील चिन्तन इसके समाधान की कुंजिका हैं। विविध उपाय दिये गये हैं। स्वयं को इच्छाओं से भिन्न और पृथक् मानना ही एक महान् तथ्य है। आप सर्व इच्छाओं एवं विचारों से सर्वथा पृथक् और भिन्न हैं। आप चैतन्य स्वरूप है। आपकी आत्मा, मन तथा इसके असंख्य भावों से अधिक गम्भीर तथा पूर्णतया परे हैं। यह रहस्यपूर्ण कुंजी है। आप मन नहीं है। स्वयं को मन से स्वतन्त्र जानो। इसका आभास अत्यन्त कठिन है; क्योंकि मन अति दृढ़ है और आपकी इसके साथ सायुज्य की वर्तमान भावना अत्यन्त पूर्ण है। सूक्ष्म विचार 'मैं' इतना छाद्मिक और स्निग्ध है कि इसका स्थिर विश्लेषण नहीं किया जा सकता और यह मौन समीक्षा से पलायन करता है, किन्तु जब आप दृढ़ाग्रह और पुनः पुनः अभ्यास द्वारा इसे ग्रहण कर लेते हैं और सूक्ष्म परीक्षण करते हैं (अथवा इसका व्यवच्छेद करते हैं) तथा स्वयं को इससे पृथक् और परे मानते हैं तब आपको गौरवशाली श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है जहाँ से आप मन का निरीक्षण कर सकते हैं। पूर्णतः अनुशासन और अनासक्ति के अभाव में आप असहाय थे। किन्तु अब, जब आप मन तथा 'मैं' भाव से दूर एक ओर खड़े हैं, आप स्वामी हैं। आप इसे साक्षी चैतन्य के रूप में इससे पृथक् देख सकते हैं।
स्व-व्यक्तित्व के सर्व भावों की समीक्षा करने की आपमें सामर्थ्य होनी चाहिए। आप अन्तःस्थल में मूक (शान्त), अनासक्त, साक्षी चैतन्य हैं। आप इन्द्रियाँ नहीं हैं; आप मन नहीं हैं; आप विचार संवेगात्मक वृत्ति अथवा भाव नहीं हैं। आप इस बुद्धि से भी परे हैं जो इस मिथ्या एकात्मक भाव के भ्रम में सम्भ्रान्त हो जाती है। आत्यन्तिक रूप में आपको इतना ही विचार करना है कि आप यह 'मैं' नहीं हैं जो आपका प्रियतम है और जिसका आप आलिंगन कर रहे हैं। यह 'मैं' अन्य विचारों की भाँति ही मन की एक वृत्ति है। वास्तविक 'मैं' (आपमें वास्तविक 'आप') एक परा मानसिक तत्त्व है। स्वभावतः चिन्तन करने वाले मन के इस 'मैं' विचार से आप सर्वथा पृथक् शुद्ध आत्मा हैं। मन से ऊपर उठो। आप शुद्ध चैतन्य हैं और आपका शाब्दिक ऐक्य 'चेतन तत्त्व' है। इस 'मैं' विचार के आप सच्चे विचारक हैं और स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए आप मन का प्रयोग करते हैं। यह चैतन्य आपके अस्तित्व का आधार रूप है जहाँ से 'मैं' विचार का उद्गम होता है। वर्तमान मोहावस्था में इसका दर्शन नहीं होता। आपकी दृष्टि पर परदा पड़ा हुआ है। जैसे ही मन 'मैं' का अवग्रहण करता है, मन पूर्वतः ही विनाशक रोगों से क्लिष्ट होता है। वेदों के अनुसार यह रोग आपकी आत्मा के ऊपर देहाध्यास है। आप सोचते हैं कि आप चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, हस्त, पाद, शिर आदि हैं। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि आप इस व्यष्टि शरीर की सीमा और बन्धन में जकड़े हुए हैं जो आपको धारण किये हुए है। इसके प्रत्येक अंग से सायुज्य प्राप्त करके इसे असीम रूप से निकृष्टतर क्यों बनायें ? शरीर यथार्थतः बन्दीगृह है और इसे असीम रूप से निकृष्टतर कह कर सम्बोधित करने का मेरा अभिप्राय मन से है जो यह कार्य करता है, 'आप' नहीं, क्योंकि आपका क्लेश मन से है जो यह मिथ्या भाव धारण किये हुए है कि 'मैं यह शरीर हूँ।' यह मन आपको सुख नहीं देगा। आप यह शरीर नहीं हैं, आप यह मन नहीं हैं; इस मिथ्या विचार को नष्ट करके ही आप सुख-प्राप्ति कर सकते हैं।
बहिर्मुखी विचारधारा को अन्तर्मुख करना मन का एक महान् विज्ञान है जो ज्ञातव्य है। मन का सहयोग न देने से प्रारम्भ करो, जब भी मन कोई कामना करे अथवा कुछ करने की इच्छा करे, अपनी स्वतन्त्रता का प्रयोग करो और कहो-"नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा", और जब भी मन कुछ करने से इनकार करे तो कहो- “तुम ऐसा करोगे।" सदा स्वयं से कहो- "मैं इस घर का स्वामी हूँ (शरीर-मन)। मैं इच्छाओं से पूर्ण मन के आधिपत्य और आज्ञा में नहीं रहूँगा। मैं आज्ञा करूँगा। मैं अपना प्रभुत्व स्थापित करूंगा और मन को मेरी बात सुननी होगी, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा।"
जैसी कि कल्पना की जाती है, मन अभिभावक नहीं है। 'मैं' के रूप में भी मन अभिभावक नहीं है; क्योंकि इसमें गतिशीलता नहीं है, यह तो केवल मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किन्तु जब 'मैं' और 'मेरा' भावों से इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं और जब कल्पना को नाटक में भूमिका दी जाती है तब अनिष्ट प्रारम्भ होने लगता है। यह कल्पना को विचारों पर अभिभूत होने की स्वतन्त्रता देना है जो उन्हें स्वशक्ति प्रदान करती है। एक विचार पर जितना अधिक चिन्तन किया जाता है, यह शक्तिशाली इच्छा के रूप में परिणत हो जाता है। अतएव मन में विचार आते ही इसका निराकरण कर दो। हिन्दू कहते हैं कि बृहत् दावानल अग्नि का व्यावर्तन हो सकता है यदि प्रारम्भ में ही छोटी-छोटी चिंगारियों को बुझा दिया जाये।
मान लो विचार, इच्छाएँ बनने की अवस्था में नहीं पहुँचता, पुनरपि आपको यह स्मरण रखने का प्रयास करते रहना चाहिए कि यह 'आप' नहीं हैं। स्वयं को इसके साथ मत जोड़ो। इसमें प्रवृत्त न हों। इसके साथ निजात्मा का सायुज्य न करो। विचार से सम्बन्ध-विच्छेद करके एक ओर खड़े हो जाओ।
यद्यपि एक ही समय पर मन में सैकड़ों विचार विचारने की क्षमता है। इसके प्रति वैज्ञानिक निश्चित धारणा यह है कि प्रदत्त क्षण में मन एक विचार सोच सकता है। यह मस्तिष्क विज्ञान की रहस्यपूर्ण विशेषता है। ससीम प्रकृति के कारण मन क्रमशः चिन्तन कर सकता है। मन इतनी द्रुतगति से सोचता है जिससे आभास होता है कि जैसे विचार समकालिक हों; किन्तु एक समय में मन में एक ही विचार रमता है।
यह तथ्य इस बात का निर्देश करता है कि यदि आप चेतना में विशेष स्वतन्त्र विचारों को जागृत करें तो उस समय मन के क्षेत्र पर किसी अन्य विचार का आधिपत्य नहीं हो सकता। स्वामी बन कर विचारों को उत्पन्न करो और आप उच्छृंखल तथा प्रकीर्ण चिन्तन के क्षय से मुक्त हो जायेंगे। तब आप व्यर्थ की कल्पना के शिकार नहीं रहेंगे। मन को संयत करो; तब अयथार्थ अथवा निषेधात्मक अन्य किसी विचार का अभिनिवेश नहीं हो सकता है।
राजयौगिक कला में चयनशील विचारधारा
मनोनिग्रह के पूर्ण विज्ञान के द्योतक महर्षि पतंजलि ने कहा है कि यदि आप किसी विचार-विशेष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको तत्काल ही विपरीत प्रकृति का विपरीत विचार जागृत करना चाहिए। उदाहरणतः यदि आपके भीतर भय का निषेधात्मक विचार है तो आप साहस का प्रत्यक्ष विचार मन में लायें। यदि आपमें घृणा और क्षुद्रता का निषेधात्मक विचार उत्पन्न हुआ है तो असन्दिग्ध रूप से तत्काल ही प्रेम, मित्रता और बन्धुत्व का विचार मन में उत्पन्न करें। स्वयं को सौहार्द भाव से परिपूर्ण करें। यदि ईर्ष्या और असहनशीलता आप पर अभिभावी है तो सहानुभूति, अवबोध और एकता के भावों को जागृत करें। किसी भी निषेधात्मक विचार की उपेक्षा हेतु किसी भी क्षण ऐसा किया जा सकता है। समुचित रूप से इस विधि के नित्य अभ्यास द्वारा इस अभ्यास की मनोवैज्ञानिक आत्मपरिणति का पूर्ण अनुक्रम समझा जा सकता है। आपके नैतिक उन्मीलन तथा उन्नति हेतु यह अमोघ आन्तरिक अनुशासन है। आध्यात्मिक जागृति में भी यह आपकी सहायता कर सकता है। यदि आप शीघ्र ही क्रोधित हो उठते हैं तो शनैः-शनैः धैर्य, प्रेम और दया के भाव मन में भरें। प्रतिदिन कुछ समय के लिए पृथक्, मौन में बैठ कर क्षमा, करुणा और दया की महिमा का चिन्तन करें। इस पर ध्यान करें। अवधानपूर्वक क्रोध के अलाभ तथा अवांछनीयता पर विचार करें। मधुर एवं सम स्वभाव के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक लाभ तथा इष्टता पर निर्विकल्प चिन्तन करें। अब्राहम लिंकन, सेन्ट फ्रांसिस, महात्मा गान्धी अथवा ईसा मसीह के उत्कृष्ट व्यक्तित्व पर ध्यान लगायें। दृढ़ अभ्यास के अनन्तर क्रोधपूर्ण विचार पूर्णतया नष्ट होने लगते हैं। मानसिक प्रवृत्तियों में पूर्ण रूप से परिणति आ जाने के कारण वे अब मन में स्थिर नहीं रह सकते।
यदि आप विवेकशील उत्कृष्ट विचारों से मन को ध्यान से नहीं भरते तो यह सदा अपने ही विचारों से स्वयं को पूरित करेगा और यह मानो मन को अपनी स्वाभाविक वन्यवृत्ति में उन्मत्त बनने की आज्ञा देने के समान होगा। मनोनिग्रह की समस्या के हल की कुंचिका है— विशिष्ट चिन्तन। विवेकशील चिन्तन मन के वशीकरण का सार है।
जब आप मन को अनुशासित और शिक्षित करने का कार्य प्रारम्भ करते हैं तब आप विचारों के सम्बन्ध में विशिष्ट होते हैं। आप मन को अपनी ही इच्छा के भद्र एवं पवित्र, युक्त एवं समुचित, स्पष्ट और हृदयंगम विचारों का भोजन प्रदान करते हैं। मन की अन्तर्दृष्टि में सदा कुछ विशेष विचार-चित्र बनाये रखो। आपको प्रेरणा प्राप्त होगी। यह विचार-चित्र आपको उन्नमित करेंगे। वे आपके भीतर एक नवीन व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। यह विचार-चित्र लिखित रूप में भी बाहर अपने समक्ष दीवार पर, मेज पर, घर में, कार्यालय में, जेब में, क्षुद्रकोष (झोला या थैली) में रखे जा सकते हैं। बाहा वृत्ति तथा आन्तरिक मानसिक दृष्टि द्वारा भी तथा चक्षु एवं विचार के द्वारा मन का पुनर्निर्माण होता है और यह नये ढाँचे में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः यह मन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। यह मनोवैज्ञानिक पुनर्जन्म है। यह आत्मा में पुनर्जन्म की क्रिया का अग्रेसर प्रतीत होता है और वस्तुतः है भी, जैसा कि ईसा मसीह ने जिज्ञासु 'निकोडेमस' के प्रश्न करने पर बताया।
इस विशिष्ट एवं विवेकशील विचार-कला का सुव्यवस्थित रूप से अभ्यास करो। शीघ्र ही आप मन के स्वभाव का पूर्णतः नवीनीकरण करने में समर्थ हो जायेंगे। आपको आभास होने लगेगा कि आप मन नहीं हैं। आप अनुभव करेंगे कि आप अन्तःकलाकार हैं जिसने मन के ढाँचे को इच्छा के अनुरूप सुन्दर स्वरूप प्रदान करण है। तक्षक (मूर्तिकार) की भाँति आपको इस पर कार्य करना है। अद्भुत प्रतिमा बनाने के लिए जिस प्रकार तक्षक पत्थर पर प्रहार करता है उसी प्रकार आपको मन पर कार्य करना है। स्मरण रहे, जब तक आप मन के साथ एक हैं, विचार की वास्तविक शालि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव स्वतन्त्र बनो। यही मनोनिग्रह की कुंचिका है।
मन को संयत करने की एक विधि-हठयोग
मनोनिग्रह की इन स्पष्ट विधियों के अतिरिक्त यह भी ज्ञान आवश्यक है कि मन तीन आन्तरिक दोलायित अवस्थाओं अथवा गतियों के वश में है जिसे यौगिक भाषा में गुण कहते हैं। वे हैं-सत्त्व, रजस् और तमस्। सत्त्व शुद्धता और प्रकाश का संचार करता है, रजोगुण आसक्ति और क्रियाशीलता उत्पन्न करता है। तमोगुण जड़ता, अन्धकार और स्थूलता का प्रतीक है। शुद्धि से मन स्थिर हो कर अन्तर्मुख होता है जब कि आसक्ति और अशुद्धि मन को अस्थिरता और संक्षोभ में प्रक्षिप्त करके इसे स्वकेन्द्र से दूर बहिर्मुख करती है। सात्त्विक मन भव्य रूप से सन्तुलित होता है। जीव को उन्नमित करने तथा प्रकृति का संशोधन करने के लिए जीवन की सभी अवस्थाओं में शुद्धि अनिवार्य है।
मन की स्थिरता को उन्नमित करने के लिए कतिपय यौगिक मुद्राओं का अभ्यास उपयोगी तथा लाभप्रद है; क्योंकि मन और शरीर का परस्पर सम्बन्ध है। यहाँ हठयोग सहायक विधि के रूप में निर्दिष्ट है। मन की अस्थिर अवस्था को परिवर्तित करने के लिए प्रातः-सायं आधा-आधा घण्टा प्रारम्भिक आसन करना भी उपयोगी है। यह आसक्ति से पवित्रता की ओर ले जाता है। शरीर को दृढ़ और सम रखना सीखने से मन संयत हो जाता है और आभ्यन्तर में एक भव्य समीकरण का जन्म होता है। ये यौगिक मुद्राएँ और सहज श्वास क्रियाएँ सब लोग सहायक रूप में मनोनिग्रह के अन्य प्रयत्नों को उन्नमित करने के लिए कर सकते हैं।
स्मरणीय प्रमुख तथ्य यह है कि मन एक साधन है। यह आपके उपयोग हेतु बना है। इसे आपने वश में रखना है। आप स्वामी हैं। ऐसे भाव का अनुभव करने से आपके भीतर शक्ति जागृत होती है। यह तथ्य सत्य है। सत्य सर्वशक्तिमान् और स्पष्ट होता है; अतएव स्वयं को सदा अप्रभावित, अनासक्त साक्षी चैतन्य स्वरूप बनाये रखो। मन को अपने से पृथक् मानो । आप शीघ्र ही इसे समझने में और जितेन्द्रिय बनने में समर्थ होंगे। ऐसा करने पर शनैः-शनैः सफलता आपके चरण चूमेगी।
यद्यपि यह दुष्कर है। पुनरपि इसे निःसन्देह नया स्वभाव बनाना है। एक बार प्रारम्भिक रहस्य का ज्ञान हो जाने पर सम्पूर्ण प्रक्रिया अत्यन्त सरल प्रतीत होने लगती है। यथार्थ विधि, उस प्रकृति के विरुद्ध इतना संघर्ष नहीं जिसे आपने परिवर्तित करना है, प्रत्युत नयी प्रकृति बनाने का प्रयास प्रारम्भ करना है जिसने पुरानी प्रकृति का स्थान लेना है। इस कार्य के प्रारम्भ होने पर पुरानी आदत नहीं रह सकती। यह एक प्रकार का कूटोपाय (वंचना) है और आश्चर्यजनक रूप से, बिना किसी प्रयास से पुरानी आदत स्वभावतः अदृश्य हो जाती है। प्रत्येक स्वभाव खण्डित किया जा सकता है और पूर्ण मन का सर्वशः नवीनीकरण किया जा सकता है।
इस नवीनीकरण की एक विशेष अवस्था में आप स्वयं को एक अत्यन्त उत्सुक एवं रुचिकर अवस्था में देखते हैं। प्रतीत होता है मानो आपके दो मन हैं- एक उच्च मन और एक निम्न, एक शुद्ध तथा एक अशुद्ध, असृजनात्मक मन। इस अवस्था तक पहुँच ही व्यक्तित्व के निषेधात्मक विचारों का अतिक्रमण करती है और केवल तभी व्यक्ति ध्यान की अवस्था तक पहुँचता है।
यदि इस वैज्ञानिक विधि का सम्यक् प्रयोग किया जाये और मानवीय व्यक्तित्व के सभी निषेधात्मक पक्षों के पूर्ण निकारण हेतु दृढ़ संकल्प किया जाये तो जीवन का आधार आत्म-संयम और धर्म बन जाये। इस पथ पर अग्रसर होते हुए, राजयोग के अनुसार, तब उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होती है जिसमें सब वृत्तियाँ बन्धनमुक्त हो जाती हैं और निम्न मन निष्क्रिय हो जाता है। आपका शुद्ध चैतन्य गौरवान्वित, आन्तरिक प्रकृति प्रशान्ति और आनन्द से परिपूर्ण हो कर प्रस्फुटित होने लगती है। मौन साक्षी चैतन्य-स्वरूप आप सत्य की अनुभूति करने लगते हैं। आपको अपनी सच्ची आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह आत्मज्ञान है- आभ्यन्तर सत्य का ज्ञान। यह ज्ञान आपको मोक्ष प्रदान करता है।
१२. सच्चे सुख का एकमात्र स्रोत
सृष्टि के प्रारम्भ से ही धरती पर सुख-प्राप्ति मानव की आकांक्षा रही है; परन्तु यह आकांक्षा समाप्त हुई प्रतीत नहीं होती। सम्पूर्ण विश्व सुख के अन्वेषण में रत है, किन्तु साथ ही हम सबको निराशा ही प्राप्त हुई। सुख की प्रतीति प्राप्त हुई नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है मानो सुख हमसे कोसों दूर है, दूर क्षितिज की ओर, जहाँ क्षितिज उस क्षण दृष्टि से ओझल हो जाता है जब हम सोचते हैं कि यह समीप है। अनेक सहस्र वर्षों के प्राचीन इतिहास के पश्चात् आधुनिक मनुष्य सच्चे सुख की अनुभूति से इतना ही दूर है जितना कि उसके पूर्वकालीन पूर्वज ! तथापि इसमें सन्देह नहीं कि सुख-प्राप्ति हेतु इस अवधि में अनेक बार घोर प्रयास किये गये हैं। शताब्दियों पर्यन्त मनुष्य ने अपने बाह्य जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रायः अथक परिश्रम करके असंख्य युक्तियों का सृजन किया है। किन्तु वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में यह सब उपाय असफल रहे हैं। क्योंकि यदि मनुष्य से प्रश्न किया जाये - "क्या तुम वास्तव में सुखी हो?" कदाचित् ही कोई मनुष्य सहज और युक्त उत्तर देगा- "हाँ, मैं सुखी हूँ।" प्रायः सभी व्यक्ति कहने लगेंगे- “ओह! मेरा विचार है..." अथवा "शायद..." अथवा "शायद इतना सुख नहीं" अथवा "मैं युक्त रूप से कह नहीं सकता...।" कुछ भी उत्तर हो, किन्तु निश्चित स्वीकार द्योतक नहीं।
यदि सभी मनुष्य शताब्दियों से सुख की खोज में निरत हैं और अभी तक उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्या इसका आशय है कि प्रापणीय कोई सुख नहीं है? क्या इसका अभिप्राय है कि सुख केवल कल्पना सृष्ट है अथवा ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, प्रत्युत हमारी अपनी ही मनोरथ सृष्टि है। या तो यह अनुमान किया जाये कि सुख मनुष्य को दुर्लभ है अथवा मनुष्य ने सुख-प्राप्ति के ग्रहण में मूलतः कोई भूल की है। कोई यह कह सकता है कि सुखान्वेषण में मनुष्य ने युक्त साधन ग्रहण नहीं किया। यदि मनुष्य कोई कार्य प्रारम्भ करता है, किन्तु अयुक्त रूप से करने पर लक्ष्य-प्राप्ति नहीं होती। एक मत के अनुसार सुखान्वेषण का स्थान अयुक्त हो सकता है। मान लो कोई वस्तु एक कक्ष में रखी है; किन्तु उसकी खोज दूसरे कक्ष में हो रही है, तो वह वस्तु प्राप्त नहीं होगी, यद्यपि वह सुनिश्चित रूप से विद्यमान है। कारण कुछ भी हो-और हम इसकी खोज करने का प्रयत्न करेंगे- ऐसा प्रतीत होता है मानो सुख ने मनुष्य को अपनी माया से वश में कर लिया है। विषयों में यह सर्वाधिक मायावी है। उसके समीप प्रतीत होते हुए भी मनुष्य को सुलभ नहीं है। क्यों? वस्तुतः क्या ऐसा ही है?
इस धरती पर होने वाली सभी अद्भुत और अति-बृहत् क्रियाएँ उसकी ओर संकेत करती हैं। उस विशेष सार्वभौमिक अभाव की ओर संकेत करती हैं जिसकी पूर्ति हेतु मानव प्रयत्नशील है। हम देखते हैं कि यह अभाव सुख की इच्छा है। यह इच्छा सकारात्मक अथवा नकारात्मक ढंग से कार्यान्वित की जा सकती है। व्यक्ति उन पदार्थों के भोग की इच्छा कर सकता है जिनके प्रति उसके मन में धारणा है कि वे सुखप्रद हैं। अथवा वह उन सब पदार्थों से छुटकारा पाने का यत्न कर सकता है जिन्हें वह सुख का विरोधी समझने लगता है। कोई भी व्यक्ति दुःख, शोक अथवा उदासी नहीं चाहता। सभी इन क्लेशों से मुक्त होने की आकांक्षा करते हैं; क्योंकि वे सुख के प्रतिपक्षी हैं। दुःख और पीड़ा से मुक्त हो कर मनुष्यों का अभिप्राय उस अवस्था को प्राप्त करना है जिसमें सुख स्पष्ट रूपेण दृष्टिगत होता है।
सुख एक अनुभव है
इतना निश्चित है। मनुष्य को अपने अभाव का ज्ञान है; किन्तु वह इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि उसकी इच्छा की वास्तविक प्रकृति क्या है और सुख उससे वंचना क्यों कर रहा है। और, एक विशेष परम आनन्द भी है जिसे जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। यह उपनिषदों, वेदों और भगवद्गीता की घोषणा है। "जान लो कि सत्य अकथनीय और सर्वोच्च मन्तव्य सुख है। वह सुख इतना बृहत् है कि बुद्धि इसका पार नहीं पा सकती और इन्द्रियाँ (जो प्रायः सुख की अनुभूति करती हैं) इसे ग्रहण भी नहीं कर सकतीं यह इतना महत् और सर्वातिशायी है।" वही सुख मानव का लक्ष्य है। पूर्णता और अखण्डता सर्वोत्कृष्ट आनन्द के लक्षण हैं। अपूर्णता इसका कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि अपूर्णता मिश्रण की सूचक है और मिश्रण तथ्यों को उपलक्षित करता है और अनुभव में समन्वय नहीं रहता। शर्करा और लवण का मिश्रण यदि जिह्वा पर कोई व्यक्ति रखे तो उसे समन्वित मिठास का सुख नहीं प्राप्त होगा; क्योंकि मिश्रण में दो तत्व निहित हैं। मिठास का स्वाद लेने के साथ ही वह विकृत मुखाकृति बनायेगा; क्योंकि लवण से भी उसका मुख भर जायेगा। स्वभाव से ही मिश्रण पवित्रता और पूर्णता का अनुभव नहीं प्रदान कर सकता। सर्वातिशायी सुख प्राप्त करना महान् लगता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति करके मनुष्य सब शोक और दुःखों का अतिक्रमण कर लेता है। सुख मनुष्य हेतु ही सुलभ अनुभव है-यह वचन मात्र सिद्धान्त के रूप में आचक्षित नहीं है। यह सारवत् आत्मानुभूत तथ्य के रूप में अधिकार रूप से उन पूर्वजों द्वारा प्रतिपादित है जिन्होंने वास्तव में उस परमानुभूति का आनन्द लिया है।
इस सुख का मूल स्रोत कहाँ है? इस स्रोत के अन्वेषणार्थ प्रगमन से पूर्व यह ज्ञान अनिवार्य है कि मनुष्य अन्वेषण किस वस्तु का कर रहा है। सुख के प्रति मत और सम्यक् विकार स्पष्ट होना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग ही अपनी अभिलाषा को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करके अपनी बुद्धि के प्रयोग का परिचय देते हैं। सम्पूर्ण विश्व किसी-न-किसी पदार्थ के पीछे भाग रहा है जिसके प्रति उसके मन में स्पष्ट ज्ञान भी नहीं है। यह सब प्रयास निरर्थक सिद्ध होता है; क्योंकि इसके पीछे बुद्धि का प्रयोग नहीं है। प्रत्यक्षीकरण करने योग्य प्रथम तत्त्व यह है कि सुख अनुभवगम्य है। यह कोई विषय नहीं है और भी, यह कोई उपलब्धि नहीं है, प्रत्युत यह आभ्यन्तर अवस्था की जागृति है जो पूर्णतः अनिवार्य है और इसलिए आपके अस्तित्व का ही अनन्यथाकरणीय अंश है। यह प्राप्य पदार्थ नहीं है जिसे किसी स्थान से लाया जाये। सुख जीव की अवस्था है। एक बार यदि यह बोध हो जाये कि यह पदार्थ सुख नहीं दे सकते तो जीवन को पदार्थों से सम्पन्न करना एक महत् भ्रम समझा जायेगा। सांसारिक पदार्थ सच्चे सुख के स्रोत नहीं हैं। अधिक-से-अधिक वे मनुष्य के कतिपय ज्ञात सार्वभौमिक असुखों और क्लेशों को किसी सन्देहात्मक स्थिति में परिवर्तित करने में समर्थ है। यह उनका एकमात्र यथार्थ मूल्य और उपयोगिता है। वे मानव द्वारा विरचित हैं और मानव स्वयं अपूर्ण हैं। वह स्वयं शोक, दुःख, पीड़ा, क्लेश का भी शिकार है। यह सर्वविदित है कि समन्वित अनुभव पूर्णता में ही सम्भव है जिसमें किसी बाह्य पदार्थ का विरोध न हो। मानव सृष्ट पदार्थों से प्राप्त मिश्रित अनुभव व्यक्ति के भौतिक भाग को भोजनादि सामग्री से पुष्ट करते हैं जो इन्द्रियों को सन्तोष प्रदान करते हैं अथवा कदाचित् व्याकुलता को दूर करते हैं; किन्तु अपूर्ण पदार्थ हमें सुख प्रदान नहीं कर सकते।
विषय-सम्पन्नता का आशय सुख नहीं
अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है : "उन भव्य पदार्थों, हृदयंगम वस्तुओं, स्वादु विषयों, रंग-बिरंगे और माधुर्यपूर्ण पदार्थों का क्या करेंगे जिनसे विश्व आपूरित है। क्या वे सुखद नहीं?" निश्चयेन ये पदार्थ सुनिश्चित अनुभव प्रदान करते हैं। किन्तु क्या ये अनुभव सुख कहे जा सकते हैं? यही हमें अब निश्चय करना है।
इन विषयों से अनुभवों की प्रबलता उनके साथ हमारे सम्पर्क पर आधारित है। उनसे सम्पर्क स्थापित किये बिना कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता। अति सुन्दर पदार्थों के प्राचुर्य से परिवेष्टित हो कर चक्षुर्निमीलन करने पर यह तथ्य निरूपित होगा। उनकी साक्षात् विद्यमानता से आप किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त करने में असमर्थ होंगे, क्यों? क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय का उनके साथ कोई सम्पर्क नहीं रहता। वे दृश्य-विषय हैं और यदि चक्षुरिन्द्रिय का उनके साथ सम्पर्क नहीं है तो कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। पुनः अत्यन्त मधुर संगीत बजने दो। कर्ण बन्द कर लो। अब आप ध्वनि का सुख न ले सकेंगे, क्योंकि आपके कर्ण और संगीत में सम्पर्क नहीं रहा। एवंविध, यावत्पर्यन्त जिह्वा भक्ष्य पदार्थ को स्पर्श नहीं करती, तावत्पर्यन्त आप सामने मेज पर रखे हुए सुस्वादु, आहार-विशेष के उत्कृष्ट विशिष्ट भोजन का आनन्द नहीं ले सकते। श्रवण, दर्शन, स्पर्श, प्राण और स्वाद-सब साधन इन्द्रियों के अनुरूप विषयों के संयोग पर निर्भर करते हैं।
शारीरिक अनुभवों की प्रकृति संवेदनशील है। अपने स्वरूप में वे इन्द्रियों के बाह्य विषयों के उपयोग के विचार और मन तक उसका ज्ञान पहुँचाने की सामर्थ्य से सीमित हैं। एक विशेष सीमा से परे जो इन्द्रिय सामर्थ्य को उपलक्षित करती है, विषय अरुचिकर और घृणास्पद बनने लगते हैं। पुनरपि, यह सत्य है, ये सब पदार्थ मन द्वारा बोधगम्य विचारों के अनुसार इन्द्रियों के संयोग से अनुभव प्राप्त करते हैं, तदपि मन की वास्तविक दशा स्पष्ट रूप से ऐसी दृष्टिगत होती है जिसमें भोग का अनुभव ही अभिभूत होता है। कतिपय विशेष अवस्थाओं में व्यक्ति को भोग की इच्छा नहीं होती। क्षण-भर के लिए मान लो, एक व्यक्ति को तार मिला कि उसका ज्येष्ठ पुत्र वायुयान-दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तब भोग्य पदार्थों की सभी प्रकार की अभिव्यक्ति उसमें किंचित मात्र भी यह भाव उत्पन्न नहीं करेगी कि इन विषयों में किसी प्रकार का सुख लिया जा सकता है। नहीं! वह किसी भी प्रकार का सुख लेने में असमर्थ होगा, क्योंकि उसका अन्तर्निहित तत्त्व, जो उसकी सुखानुभूति में अनिवार्य है, वह मन की दशा से अभिभूत है। संसार के सभी विषय भी उसे सुखानुभव नहीं प्रदान कर सके।
अतः यह कोई अचम्भा नहीं यदि समृद्धि और कष्ट प्रायः साथ-साथ रहें। कुछ लोग विषय-भोग के सब पदार्थों से सम्पन्न होते हुए भी दुःखमय जीवन व्यतीत करते हैं। उनका मन शान्त नहीं। वे निराश अथवा दुःखी रहते हैं। वे अपने जीवन को समाप्त करने का भी विचार करते हैं। क्यों? यही उत्तर है कि पदार्थों की प्रचुरता और उससे प्राम होने वाले सुख-रूपी अनुभव का इतरेतर कोई नित्य हेतुक सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत भी दशा स्पष्ट है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अत्यल्प पदार्थ हैं; किन्तु फिर भी वे प्रसन्न हैं, सुखी है। वे सदा हँसमुख रहते हैं, कार्य करते समय भी गाते रहते हैं। ऐसा क्यों? यदि बाह्य पदार्थ सुखानुभूति हेतु अपरिहार्य हैं तो निर्धन लोग, फटे-पुराने वस्त्र ओढ़े हुए अथवा जूर्ती के नवीकरण की नितान्त आवश्यकता में हैं; किन्तु पुनरपि वे प्रसन्नचित्त हैं-ऐसा क्यों? यदि पदार्थों की विद्यमानता सुख के लिए पूर्वाकांक्षित हो तो उनकी अविद्यमानता लोगों के सर्वसुखों का हरण कर ले।
एवंविध विषयों की अविद्यमानता सुखानुभूति के अनुरूप पायी गयी है जिस प्रकार विषयों की विद्यमानता दुःखानुभूति के अनुरूप देखी गयी है, यह स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि विश्व के पदार्थों और सुखानुभूति में कोई हेतुक सम्बन्ध नहीं है।
सुख-एक खोयी हुई पूँजी
प्रायः सर्व आकांक्षित वस्तुओं से सम्पन्न व्यक्ति कुछ दिन अपने कार्य से मुक्त होने पर किस प्रकार आचरण करते हैं। वे पर्वतों पर जाते हैं अथवा राष्ट्रीय उद्यानों अथवा हवाई में जाते होंगे। यद्यपि उनके पास वे सर्व पदार्थ हैं जिन्हें प्रायः सुख-स्रोत माना जाता है। तथापि अल्पकाल के लिए कार्यमुक्त होने पर वे वस्तुतः उन सबसे दूर भागने का यत्न करते हैं जो पूर्णतः उनके पास विद्यमान हैं। इन वस्तुओं के महत्त्व पर कौन विचार करता है? उनका परिणाम कौन देखता है? विवेकशील व्यक्ति को यह भलीभाँति ज्ञात है कि भौतिक पदार्थों में मनुष्य को अल्प मात्र भी सुखानुभूति प्रदान करने की शक्ति नहीं है। तब इस अभिव्यक्ति का विशेष महत्त्व क्या है? सुख का अन्वेषण अथवा 'सुख की खोज'? हम खोज और अन्वेषण शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? आकांक्षा अथवा अन्वेषण का अभिप्राय है-कुछ खो गया है। यदि कोई वस्तु थी, अब नहीं है, हम तत्काल उसकी खोज में निकलते हैं। खोयी हुई वस्तु की उपलब्धि सहज रूप से पुनर्प्राप्ति है। अतएव, जीवन सुख-स्रोत के अन्वेषणार्थ संघर्ष नहीं, प्रत्युत बीते सुख को पुनः प्राप्त करने का उपाय है। अन्वेषण के रूप में, जीवन एक उद्यम है-उस वस्तु को प्राप्त करने का जो हमसे लुप्त हो चुकी है।
यह तथ्य हमें और भी सूक्ष्म लक्ष्य और उच्चतर समन्वय की ओर ले आता है। यदि सुख एक अवस्था है जो कभी आपके पास थी और अब लुप्त हो चुकी है तो उस लुप्त हुए तत्त्व की पुनः प्राप्ति क्यों? सुखानुभूति हेतु आप उस अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते थे। यह तत्त्व कहाँ रहता है? यह तत्त्व आपके भीतर विद्यमान है। यह आपके बाहर नहीं। तब यह किस सम्बन्ध में विद्यमान है यह आपका अंश है अथवा आपके संसर्ग में है? अथवा यह आपका अभिन्न रूप है? आप स्वयं वह सुख हैं। सुख आपकी अनिवार्य प्रकृति है। सुख आपकी आभ्यन्तर प्रकृति है। आप इसे कभी खो नहीं सकते; क्योंकि यह आपका अनन्य रूप है।
सुख का अभाव और तदर्थ उसकी खोज की वर्तमान क्षणिक अवस्था विस्मृति की अवस्था है, सुखों के वास्तविक लोप की नहीं। दर्शनशास्त्र में इसकी विविध प्रकार की व्याख्या दी गयी है। तरुणावस्था में कदाचित् मैं जब तृतीय कक्षा में था, उस समय हमारी अँगरेजी भाषा की पाठ्य-पुस्तक में एक अत्यन्त भावपूर्ण छोटा-सा पाठ था जिसका अर्थ है- "दादा की ऐनक।" इसमें एक सदन के स्वागत-कक्ष के कलरव से परिचय दिया जाता है, जिसमें दादा ने अपनी ऐनक खो दी और पोतों आदि की पूर्ण सन्तति को इसकी खोज में लगा दिया। जोन, पीटर, जो और जौन-और खोज जारी है। वे सोफे के नीचे देखते हैं, कालीन के ऊपर और शेल्फ के ऊपर चढ़ कर पितामह के तकिये के पीछे झाँकते हैं।
कुछ समय की खोज के उपरान्त जब पितामह अधिकाधिक धीरज खोने लगते हैं, छोटा टॉमी जो सब खोज करता रहा और न मिलने से निराश होने लगा, अकस्मात् चिल्ला उठा- "पितामह, स्मरण कीजिए-सोने से पूर्व आपने उसे कहाँ रखा था।" और फिर जब वह पितामह की ओर निहारता है- देखो! वह तो पितामह के मस्तक पर ही शोभायमान है। वह पूर्ण समय वहीं पर थी, खोयी तो थी नहीं। ऐसा आभास हुआ कि वह खो गयी है; क्योंकि पितामह भूल गये थे। समाचारपत्रावलोकन के पश्चात् उन्होंने अवचेतन मन से उसे मस्तक पर ही धकेल दिया था।
सुख की खोज की अवस्था में आपकी दशा भी ऐसी ही है। आपकी आत्मा की प्रकृति ही अनिर्वचनीय, अक्षय्य और अविकारी, निष्कलंक सुख है। सुख का अभाव एक प्रकार से किसी विषय का लोप नहीं है, प्रत्युत इसकी आभ्यन्तर विद्यमानता के प्रति आपकी जागृति का अभाव है। सुख-स्रोत आपके भीतर ही है। सुख का वास्तविक स्रोत आपके अन्तःकरण में ही विराजमान है। आपकी आत्मा ही आपके सुख का मूल है। यावत्पर्यन्त मनुष्य अपनी प्रकृति का साक्षात्कार नहीं करता और मूल में उसकी खोज नहीं करता। क्या वह सुख से पूर्णतया वंचित न रहेगा ? निश्चयेन! जैसे आप अपने लिए किसी सुख की अनुभूति हेतु अगणित साधनों का उपयोग कर सकते हैं। वे साधन क्या है? अत्यन्त सरल उपाय है। आप उन सभी तत्त्वों से छुटकारा पा सकते हैं जो आपके सुख का अपहरण करते हैं। अधिकांशतः यह चेष्टा निषेधात्मक है, क्योंकि सुख की प्राप्ति हेतु आप प्रत्यक्ष कार्य नहीं करते। आप अनुमान लगा लेते हैं कि सुख अमुक वस्तु में है, परन्तु उसका अनुभव नहीं किया गया होता। तब आप स्तम्भित होते हैं कि उस अनुभव को कोई रोक रहा है और आप विघ्नों के निराकरण हेतु अग्रसर होते हैं और यह दशा होती है। यदि प्रकाश विद्यमान है और किसी प्रकार आवरण डाल दिया गया है तो प्रकाश पाने के लिए आपको आवरण हटाना होगा। किसी स्थान पर यदि स्वर्ण दबा हुआ है तो उस स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए आपको बाधक मृत्तिका, पत्थर और कंकड़ हटाने होंगे। तब आपको स्वर्ण मिलेगा। वे कौन-कौन से तत्त्व हैं जो हमें सुख से वंचित करते हैं? वे हमारी अपनी ही सृष्टि हैं। वे मनुष्य की मूल भूल के कारण हैं, जो विचार में समायी हुई है कि सुख विषयों से ही प्राप्त होता है। और उस भ्रान्त विचार के कारण ही उन सब तत्त्वों का जन्म हुआ जो मनुष्य की वंचना की सृष्टि है।
इस मूल भ्रान्ति से जागृत होने वाले इच्छा और कामना मानसिक शान्ति का विनाश कर देते हैं। मानसिक शान्ति के न होने पर सुख कहाँ से आ सकता है? सुख मन की शान्ति पर निर्भर है। मन की उस प्रशान्त मौन अवस्था में सुख उत्पन्न होता है; क्योंकि सच्चा सुख आपकी आन्तरिक आध्यात्मिक अवस्था है। सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश एकमात्र माध्यम जिसके द्वारा यह अभिव्यक्त हो सकता है, वे हैं बुद्धि और मन। यदि ये दोनों माध्यम उद्वेग की ऐसी अवस्था में प्रक्षिप्त कर दिये जायें कि वे इस आभ्यन्तर सुख की वृद्धि हेतु समुचित स्रोत न बन सकें तो उसकी दशा अयोग्य और प्रतिकूल हो जाती है। मन और बुद्धि में शान्ति और अनुद्वेग होने पर ही आन्तरिक सुख प्रकट होता है। बाह्य विषयों से ही सुख प्राप्त हो सकते हैं- आपकी इस मूल भ्रान्ति से उत्पन्न होने वाली इच्छाएँ और अभाव की भावना ही आपकी शान्ति और सफलता की अपहर्ता हैं। इस भूल से आप जीवन प्रारम्भ करते हैं। शैशव काल से यह शिक्षण दिया जाता है कि समय अच्छा व्यतीत करने का अभिप्राय है किसी स्थान पर जाना, कुछ करना, वस्तु खरीदना और शिशु इसी भ्रान्ति में ही पलते हैं। प्रौढ़ावस्था में वह अपने से बाह्य पदार्थों की दया पर रहता है। इस संसार के यथार्थ बोध का स्वल्प ज्ञान भी जैसा कि यह वास्तव में है, युवकों में भर देने से सुख और आनन्द के रूप में समृद्धि प्रदान करेगा।
इन्द्रिय-विषयों का सीमित उपयोग
विषयों के वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन करने की चेष्टा करो। इस धरती पर उपयुक्त जीवन-यापन हेतु व्यक्ति को पदार्थों के सीमित मूल्य का निरूपण करना होगा। कतिपय पदार्थ जीवन के पोषण हेतु अनिवार्य हैं। उनका उपयोग उल्ली सीमा तक होना चाहिए। किन्तु उन्हें अपने जीवन में अनुचित महत्त्व ग्रहण न करने दो; क्योंकि कार्य करने की अपेक्षा वे सच्ची शान्ति और सन्तोष के मार्ग में निश्चित रूप से उपद्रवी तत्त्व न बन जायें।
इस प्रकार आपका सुख इन पदार्थों के अधीन हो जाये। यह सब पदार्थ इस प्रकार अपना आधिपत्य जमा कर आपको वशीभूत कर अपना दास बना सकते हैं। मानव के लिए इन पदार्थों का समुचित बोध और उनके स्वरूप का सम्यक् मूल्यांकन तथा उनके उपयोग का सही ज्ञान रखना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जब वि षय आपके अन्तःकरण पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करें तो आपको कहना चाहिए- "बस, इससे अधिक नहीं।"
समय की कसौटी पर खरे उतरे-सुख के साधन
जीवन को यथासम्भव सादा बनाने का प्रयास करो। जीवन की सरलता सुख का वास्तविक रहस्य है। सुख का अप्रतिबद्ध अबाधित अनुभव जिसका आवास अन्तःकरण में है सादगी से उद्भूत होता है। अतैव अपने जीवन को विषय-वैपुल्य से जटिल मत बनाओ। पदार्थों की विपुलता तथा अनन्त इच्छाओं के कारण दुर्भाग्यवश आधुनिक मानव ने अपना सुख खो दिया है। आपने पैन अमेरिकन एयरलाइन्स, TWA आदि के चमकदार प्रकाशित पोस्टर देखे होंगे। जिस 'स्वर्ग' का वे अवकाश के लिए प्रचार करते हैं वह अमरीका के राजधानीय शहरों में नहीं, वरन् दक्षिण सागर के द्वीपों में है। क्यों? यद्यपि इन स्थानों पर विशाल रंगमंच, जलपान-स्थल और घुड़दौड़ मार्ग कदापि नहीं हैं। साधारण मनोरंजन के साधन कदाचित् ही उपलब्ध हैं। तथापि मनुष्य तत्काल उस स्थान को स्वर्ग मानता है, क्योंकि मनुष्य को उन स्थानों के प्राकृतिक सौन्दर्य का आभास है। हवाई का आदिवासी वहाँ सर्वदा नृत्य करता और गाता है। वह अपेक्षाकृत निश्चिन्त और सरलता तथा सन्तोष के सुख से आप्लावित होता है। हम उससे ईर्ष्या करते हैं और कम-से-कम उस समय के लिए सब विक्षेपों को त्याग कर उसके स्थान पर जा कर उसका अनुकरण करने की भी चेष्टा करते हैं। सरलता ही सुख का मूल है।
अनिच्छा से भी आधुनिक मनुष्य अपने जीवन को इतना जटिल बना लेता है। उसे विदित है कि सरलता सुख का रहस्य है। "किन्तु मैं विवश हूँ!" ऐसा कहते हुए वह क्रन्दन करता है। वह अद्भुत स्वर्ग को भी विस्मृत करने का प्रयास करता है। वह किसी सुप्रसाधित शाला अथवा मदिरागृह में जाता है। वह अपनी वर्तमान दशा की अक्षमता को किसी भी प्रकार से कुछ भी करके विस्मृत करना चाहता है।
आन्तरिक परिस्थितियों के अनुसार ही उसमें से सुख प्राप्त करने की क्षमता रखो। प्रतिज्ञा करो-परिस्थिति में शक्ति नहीं है कि मेरे अनुभव को परिणत कर दे। मेरा अनुभव केवल उतनी मात्रा तक परिवर्तनीय है जितना मैं उसे परिवर्तन की आज्ञा देता हूँ। यदि मैं कहूँ नहीं, तो परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे वही सुख-सन्तोष प्राप्त रहता है।
यह प्रति घण्टे में परिवर्तित हो सकती है। किन्तु मैं पुनरपि अपरिवर्तनशील रह सकता हूँ। सरलता और सन्तोष में अत्यन्त आनन्द की वृष्टि होती है। सर्वप्रथम आप ऋण मुक्त रहेंगे। ऋण-भाग अथवा ऋण योजना का क्रम जो प्रतिमास और प्रतिवर्ष आता है वह समाप्त हो जायेगा। कुछ लोग सर्वथा स्वतन्त्र नहीं हैं। वे उन कम्पनियों के दास बन जाते हैं जिनसे वह किश्तें प्रारम्भ करते हैं। वे अपने मकान, कार, रेडियो, टेलिवीजन, रैफरिजरेटर, वस्त्रप्रक्षालनयन्त्र अथवा परमात्मा जानता है कितने उपकरणों का आविष्कार हो चुका है, जिनका वह जीवन पर्यन्त अंशाशतः ऋण-भार चुकाते रहते हैं।
एक सरल और सन्तुष्ट जीवन मानव-निर्मित पदार्थों की अपेक्षा ईश्वर-निर्मित पदार्थों पर अधिक निर्भर करता है। सैकड़ों पदार्थ आपको प्रफुल्लित कर सकते हैं यदि आप उन्हें देखने की क्षमता रखते हों तो। आप प्रातःकाल अपने कक्ष से बाहर आ कर अरुणोदय का अवलोकन कर सुख प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय पर और अधिक सुख की अनुभूति होती है। विहंग गान श्रवण और भी अधिक सुखद होता है। शीतल मन्दानिल के अनुभव का तो कहना ही क्या? सुख की सीमा नहीं है। उषा-काल, सूर्योदय, विहंग, बच्चों की हँसी, भव्य नील वर्ण आकाश, बड़े-बड़े समुद्री जहाजों की भाँति चलते हुए श्वेत मेघ, नृत्य करते हुए पुष्प आदि में आप सुख खोजने का प्रयास करें। यदि आप सुख लेना जानते हैं तो वे आपको प्रेरित करेंगे। इस रहस्य का उन्मीलन करने पर आपके सुख की सीमा न होगी।
और भी अन्य जनों के सुख से भी सुखानुभूति प्राप्त करना सीखो। ईर्ष्यालु बनने की अपेक्षा अन्यों के सुख में आनन्दित हो जाओ। दूसरों की प्रसन्नता देख कर प्रसन्न हो जाओ। दूसरों के जीवन में सुख-संचार करके सुखी होना सीखो। दूसरों को प्रफुल्लित करके स्वयं प्रफुल्लित होने की कला सीखो। आपका सुख सहस्र गुणित हो जायेगा। वर्तमान क्षण में आपके अपने ही अनुभवों द्वारा (सुख) संकुचित हो गया है। किन्तु यदि आप सर्व अन्य जनों से सुख प्राप्त करना आरम्भ कर देते हैं तो आप नित्य रूप से सुखी हो जायेंगे। किसी का भी सुख आपके सुख का अंश बन जायेगा, आपके सुख को और गुणित करेगा।
केवल अपनी सम्पन्नता से ही नहीं, प्रत्युत सब पदार्थों के सौन्दर्य में से सुख का निष्कर्ष करो। इस प्रकार से आप सुखार्थ सार्वभौम क्षमता का विकास करेंगे। अपने कोष के पैसे का बिना स्पर्श किये आप सुख की असीम पूँजी का साक्षात्कार करेंगे जो आपके चारों ओर प्रत्येक स्थान पर बिखरी हुई है। प्रभुप्रदत्त अपार पदार्थों का अनुभव करने पर जिनको पा कर अथवा देख कर हम प्रसन्न होते हैं, सम्पूर्ण दिवस भी उसका धन्यवाद करते-करते पर्याप्त न होगा। अवर्णीय पूँजी उसने प्रदान की है। अपने शरीर का, अपनी आत्मा का ही ध्यान कीजिए। आपके पास दो प्रबल चक्षु हैं। मान लो, कोई कहता है- "मैं तुम्हें बीस सहस्र रुपये दूँगा, मुझे एक चक्षु दे दो।" मस्तिष्क की निरामयावस्था में कौन मनुष्य इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा? आपको यदि शत सहस्र रुपये दिये जायें तो बदले में क्या आप जीभ दे देंगे? इसका अभिप्राय यह है कि आपके पास करोड़ों के मूल्य के पदार्थ हैं। पूर्णतः विद्यमान पदार्थों के मूल्य का आभास न करते हुए इतने पर भी अल्प विषयक पदार्थों के लिए जो हमारे पास नहीं हैं, हम विषण्ण और क्षुब्ध हैं। अभाग्यवश कुछ लोग इन पदार्थों से वंचित भी हैं। उनकी अपेक्षा आप कितने भाग्यशाली हैं। यदि केवल आप इतना ही चिन्तन करें कि प्रभु ने आपको कितना दिया है तो आपके जीवन का दृष्टिकोण ही परिणत हो जायेगा। इन अल्प रहस्यों को पहचानो। वे अल्प हैं; परन्तु अति महत्त्वपूर्ण हैं। वे प्रकाश और अन्धकार का सा अन्तर ला सकते हैं।
जीवन से प्राप्त अनुभवों को स्वीकार करना सीखो। उन पर क्षुब्ध, क्रुद्ध और व्यथित होने से कोई लाभ नहीं। इन अनुभवों से प्राप्त दुःख में आप और अधिक दुःख जोड़ देते हैं। शान्त और बुद्धिमत्तापूर्ण परित्याग भाव रखो। इहलोक में मानव-जीवन को पथ-प्रदर्शित करने वाली एक पराशक्ति मेधा है और यह अनुभव जो उसी स्रोत से निःसृत होते हैं, उन्हें मनुष्य की ही भाँति स्वीकार करना सीखो। जीवन में आने वाले छोटे-छोटे कष्टों को सहन करो। अल्प विपदा आने पर सहन करो और इसकी व्यथा से मुक्त होना सीखो । एवंविध दुःखद तथा अप्रिय अनुभवों द्वारा भी आप अपने जीवन को समृद्ध और सुखी कर सकते हैं।
सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करो। अपने से बड़ों के प्रति दाक्षिण्य भाव रखो। उनके समक्ष भीरु, संत्रस्त और सुधीर न बन जाओ। इससे भी आपका सुख लुट जायेगा। प्रसन्नचेतस् रहो। अपने साथ के लोगों से मैत्री रखो। सबसे अनन्य भाव की अनुभूति करो। पद, स्वास्थ्य, बल, सौन्दर्य आदि में अपने से अघर व्यक्तियों के प्रति करुणा, प्रेम और दया का भाव रखो। दुष्ट, कपटी, अप्रिय और कुत्सित जनों से विरक्त रहो। स्वयं को रोष, क्लेश, शत्रु भाव अथवा घृणा की स्थिति तक मत लाओ। दुष्ट की उपेक्षा करो। निम्नलिखित चार साधन व्याकुलता से आपकी रक्षा करेंगे-अपने से ज्येष्ठ जनों के प्रति सम्मान, समान आयु वालों के साथ बन्धुत्व और मैत्री भाव, अपने से निम्न के प्रति करुणा और दया भाव और दुःखावह, कुत्सित, दुर्जन, कपटी तथा शत्रु भाव रखने वालों के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव! जीवन में इन चार प्रकार के लोगों से आपका सामना होता है।
सर्वोपरि, क्रोध को स्थान मत दो। संसार में क्रोध ही अन्य किसी भी तत्त्व की अपेक्षा अधिक सुख का विनाशक है। यह घर की सम्पूर्ण प्रसन्नता को विशीर्ण कर सकता है। यदि घर में एक सदस्य भी क्रोधी स्वभाव का है और क्रोध करता है तो वह घर के सभी सदस्यों की प्रसन्नता का अपहरण कर सकता है। सहवासी भी अभिभूत हो
इन्द्रियों पर विवेकपूर्ण संयम स्थापित करो। कामिक सम्भोग की उत्तेजना मानव का स्वाभाविक अंग है; किन्तु यह आपकी प्रकृति के मनो-शारीरिक भाग से ही सम्बन्धित है। इस रूप में हमें इसका बोध करना है। पुनरपि इन्द्रियों को वशीभूत करने के लिए मेधायुक्त होना प्रत्येक व्यक्ति का विशेष अधिकार है। इस प्रकार से इन्द्रियाँ सुख का नाश नहीं कर सकतीं। यदि उन्हें आप पर आधिपत्य जमाने की आज्ञा दे दी जाये तो आप कदापि सुखी नहीं रह सकते। यह विधि का विधान है।
जीवन को धर्म, सत्य और पवित्रता पर आधारित करो। यदि पवित्रता आपका पथ-प्रदर्शक नियम है तो दोष, संकीर्णता और मानसिक विक्षेप का अभाव रहेगा और मनोवैज्ञानिक आपके लिए अनावश्यक सिद्ध होंगे। धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने वालों का जीवन सुखमय होता है। यथा, सुख दिव्यस्वरूप परमात्मा का गुण है, तथैव धर्म प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से उद्भूत है। यद्यपि प्रारम्भ में यह कठिन प्रतीत हो सकता है, तथापि धर्म और सत्य के अनुरूप जीवन बनाने से आप कितनी ही कठिनाइयों का अतिक्रमण करेंगे। इसे प्रमाणित करने के लिए यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपको अनेकों झूठ बोलने पड़ेंगे। सत्य पर अडिग रहने से आपकी अनेक चिन्ताएँ और सहस्रों विघ्न दूर होते हैं। आज के युग में सत्य और पवित्र जीवन, उन तत्त्वों से बचा हुआ है जो जीवन में शोक और दुःख का संचार करने वाले होते हैं।
और भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि आप सर्वसुख, हर्ष और आनन्द के उस महान् आभ्यन्तर स्रोत की सन्निधि प्राप्त करें।
आप स्वेच्छापूर्वक उसे किसी भी नाम से पुकारें, मैं इसे कोई नाम नहीं देना चाहता। उसे अपने अस्तित्व का केन्द्र बनाओ। यही शाश्वत तत्त्व है जो आपके जीवन का आधार है। यही आपका अल्फा और उमेगा अर्थात् सर्वस्व है, आपका आश्रय, निर्दिष्ट स्थान और लक्ष्य है। प्रेम-संवर्धन द्वारा इसका सान्निध्य करो। परम पिता परमात्मा से प्रेम करो। परम ब्रह्म परमात्मा को सदा स्मरण करो। सुख और आनन्द की इस परम आनन्दप्रद अवस्था में सदा के लिए लीन होने वाले तत्त्वज्ञानियों ने महान् रहस्योन्मीलन द्वारा हमें सुख-प्राप्ति का अचूक साधन प्रदान किया है। वह रहस्य है दिव्य नाम। उन्होंने कहा- "दिव्य नाम जप का अभ्यास करो। परमात्मा के नाम और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वे एक ही हैं। यदि आपके अन्तःकरण में दिव्य नाम है तो मान लो परमात्मा ही आभ्यन्तर में विराजमान है।" यह एक महान् आध्यात्मिक सत्य है। यह एक महान् तथ्य है। इसे यदि आप स्मृतिपटल पर उतार लें और दिव्य नाम को अपना बनाने का प्रयत्न करें और यदि आप सर्वदा दिव्य नाम का जप करते रहें, दिव्य नाम का आह्वान करें और स्वयं को सदा दिव्य नाम की धारा से पूर्ण करें तो आप सदा प्रसन्नचित्त और आनन्दित रहेंगे।
अत्यन्त सच्चे शब्दों में सुख आपके भीतर ही विद्यमान अपरिवर्तनीय अनुभव है। यह वह जागृति है जिसकी विद्यमानता आपको अन्य सब पदार्थों से माधुर्य प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान करती है और जिसकी अविद्यमानता आपको किसी भी विषय के माधुर्य से वंचित करती है। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।
यह गणित में अंक '१' का कार्य करती हैं। अंक '१' के आगे आप कितने ही शून्य लगाते जायें, प्रत्येक शून्य असाधारण रूप से अंक के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा; किन्तु '१' अंक के वहाँ न होने पर सब शून्य निरर्थक हैं। उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। इसी प्रकार से सभी पदार्थ उस एक सत्ता की विद्यमानता में ही सुख प्रदान करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। उसे अपने जीवन का केन्द्र-बिन्दु बनाओ। उसे अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ और विशिष्ट स्थान दो। तब आप क्षण-भर के लिए भी अपने सुख से वंचित न रहेंगे। आपको उससे दूर ले जाने में किसी की क्षमता न होगी; क्योंकि आप स्वयं ही उस सुख में विराजमान् हैं। मछली को किसी छोटे पात्र से बाहर ला कर यदि सागर में छोड़ दिया जाये तो वह स्वेच्छापूर्वक कहीं भी तैरती है और सदा उस विशाल सागर में रहती है। आओ, सम्भ्रान्त जीवन रूपी अल्प पात्र से जहाँ हमने बाह्य पदार्थों को अभिनिवेश दे रखा है, स्वयं को निकाल कर बाहर करें और उस विशाल सुमहत् सत्य में प्रवेश करें। परमात्मा में सुख है और परमात्मा मेरे भीतर है। वह और मैं एक हैं।
आभ्यन्तर में ही शाश्वत सुख का अक्षय स्रोत प्रवाहित हो रहा है। आप इसी सत्य में अपना जीवन व्यतीत करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीवन सुख-स्रोत का प्रवाह बन जायेगा। ईश्वर करे, आपका जीवन अश्रुधारा के रूप में नहीं, वरन् अनन्त सुख की अक्षय्य धारा के रूप में प्रवाहित हो। यही मेरी प्रार्थना है। भगवान् आपको शक्ति और प्रेरणा प्रदान करे, जिससे आप उस सारल्य और सन्तोष, उस देदीप्यमान् और कान्तिमान् धर्म (गुण) अनासक्ति की निरीह अवस्था और सब प्राणियों के साथ मैत्रीभाव को विकसित करें जिससे यह महान् उपहार जो आपकी प्रतीक्षा में है, आपका अपना बन जाये। आपका जीवन आनन्द की किरणों से ज्योतित हो ।
१३. योग की सत्यता
यह गमनशील संसार नाम और रूपों से बना है। इसमें सब वस्तुएँ परिवर्तित हो कर अचिरेण विलय को प्राप्त होती हैं; किन्तु सम्पूर्ण परिणति क्रम में एक वस्तु स्थायी रूपेण अपरिवर्तनशील है। यह है महान् सत्य, अविनाशी, अनश्वर, अविकारी सत्ता जिसे आप ब्रह्म कहते हैं। यह महान् सत्ता समस्त प्राणियों का सार्वभौम शाश्वत स्रोत, आधार एवं आत्यन्तिक लक्ष्य है। वह शाश्वत परम ज्ञान, असीम आनन्द, अपरिमित और अक्षय्य शान्ति है। उसे प्राप्त करने पर मनुष्य निर्भय, मुक्त और नित्य स्वरूप हो जाता है। उसके साक्षात्कार द्वारा आप मृत्युंजयी बन कर शोक, दुःख और पीड़ा से ऊपर उठ जाते हैं। आप सुख, अक्षय्य शान्ति तथा आनन्द और मोक्ष की अनिर्वचनीय, प्रशान्त एवं परमोत्कृष्ट चैतन्यावस्था को प्राप्त करते हैं। स्पष्टतः और सारतः यह वैसे ही सम्भव है जैसे एक पके हुए फल का उत्पाटन (तोड़ना), चखना और आनन्द लेना।
योग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके असीम आनन्द की अनुभूति प्राप्त करता है जो अविकल, अमिश्रित और सम्पूर्ण है। दिव्यता की ओर अभिगमन योग है। योग शब्द का यह सरलतम अभिप्राय है। यह सत्य पर आरोहण अथवा शाश्वत पूर्ण सत्ता की ओर गमन है। योग का विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस विज्ञान का उद्भेद पावन भारत भूमि के प्राचीन ऋषियों-मुनियों ने किया और सर्वकालों के लिए इसे मानवता को प्रदान किया। इस सार्वभौमिक पैतृक अधिकार का सम्यक् बोध निश्चयेन आत्मज्ञान हेतु एक विशाल पाद-न्यास होगा। इस महत् विज्ञान का यथार्थ मूल्यांकन आपको अधिकाधिक सन्तुष्ट रूप से जीवन यापन करने की सामर्थ्य प्रदान करेगा।
पूर्वीय ज्ञान
महती बीसवीं शताब्दी की इस वर्तमान वेला में 'एक विश्व-मत' विवेकशील पुरुषों के हृदयों में स्थान ले रहा है। सांस्कृतिक मूल्यों एवं वैज्ञानिक ज्ञान तथा मानव-जीवन के अन्य अनेक पक्षों में आदान-प्रदान तथा परस्पर-विनिमय की अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है। विविध जातियों एवं राष्ट्रों की उपलब्धियाँ सम्पूर्ण विश्व की सामान्य पूँजी बन रही है। सर्वत्र जनगण मानवता की एकता के प्रति अधिकाधिक सजग हो रहे हैं।
यह स्पष्ट है कि जहाँ मानव-जीवन के बाह्य क्षेत्र में (पाश्चात्य) देशों ने अनेक अद्भुत आविष्कार किये हैं वहाँ पूर्वीय देशों ने और विशेष रूप से भारत ने मनुष्य के अन्तः-जीवन के क्षेत्र में अद्भुत उद्भेदन किये हैं। पूर्वी और प्रतीची दोनों की उपलब्धियों के संयोग से दोनों को लाभ होगा। यदि आप पाश्चात्यवासी पूर्व की महान् पूँजी और ज्ञान को प्राप्त कर लें और अपने आन्तरिक जीवन की सम्पूर्णता हेतु व्यावहारिक विधियाँ ग्रहण कर लें और हम पूर्वीय यदि पाश्चात्य बाह्य भौतिक विज्ञान की उन्नति और अभ्युदय से लाभ ग्रहण कर लें तो विश्व में एक नवीन सामंजस्य स्थापित हो जायेगा। इस सन्दर्भ में, योग का विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस समय यह स्पष्ट करना और भी अधिक अनिवार्य है कि इस महाविज्ञान का विषय क्या है; क्योंकि इसके सम्बन्ध में अनेकानेक मिथ्यावाद प्रचलित हैं जो निरर्थक से असंगत (विलक्षण) आदि विभिन्न उपाधियाँ प्राप्त किये हुए हैं। अतः मैं योग के सम्बन्ध में यथा-सम्भव स्पष्ट एवं सत्य विचार प्रस्तुत करने तथा इस महती विशिष्ट बीसवीं शताब्दी में व्यक्तिगत रूप से इसके महत्त्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा।
योग क्या नहीं है
प्रथमतः एवं प्रधानतः योग केवल सूत्र-श्रृंखला ही नहीं है। योग के सम्बन्ध में कुछ विलक्षण मत प्रचलित हैं मानो मूलतः यह शरीर की विविध विलक्षित स्थितियों से सम्बद्ध हो जैसे-शीर्ष के बल खड़े होना, मेरुदण्ड को मोड़ना अथवा योग के विषय में प्रकाशित पुस्तकों में चित्रित किसी भी असंगत मुद्रा को ग्रहण करना-ये कलाएँ योगाभ्यास के एक ही प्रकार के लक्षण में प्रतिपादित होती हैं, किन्तु वे अत्यन्त अनिवार्य लक्षण रूप नहीं हैं। यह सम्भव है कि इन मुद्राओं के सम्बन्ध में किंचिदपि ज्ञान न होने पर भी योगी पूर्ण हो सकता है। मुद्राओं का अभ्यास योग का अनिवार्य अंग नहीं है। अधिक-से-अधिक सम्यक्-योग में ये मुद्राएँ प्रारम्भिक अथवा अल्प सहायता करती हैं।
द्वितीयतः योग चमत्कारिक क्रियाओं का अनुष्ठान नहीं है। मैं इसकी व्याख्या विशेष रूप से दे रहा हूँ; क्योंकि अभाग्यवश पूर्व के कतिपय छद्धी योगियों द्वारा प्रसारित मिथ्यादेशों द्वारा पाश्चात्य देशों में ऐसे भ्रम हो गये हैं। सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे लज्जा नहीं है। गत पचास वर्षों में पश्चिम में अनेक महान् स्वामी और योगी आये हैं; किन्तु उनमें अनेक मिथ्या चिकित्सक और छद्मी भी आये हैं। इस विज्ञान के सम्बन्ध में बिना किसी अधिकार के उन्होंने मात्र विश्रामप्रद जीवन यापन करने अथवा किसी अन्य स्वार्थ की पूर्ति हेतु योगी बनने का ढोंग रचा है। उन्होंने पश्चिम के अनेक सच्चे साधकों को भीषण रूप से सभ्रान्त किया। वे बहुत पहले आये और अभी भी विद्यमान हैं। दुर्भाग्यवश, प्रत्येक भद्र वस्तु को दुष्टजन सदा भ्रष्ट कर देते हैं। इतिहास में सर्वकालों में और समस्त विश्व में ऐसा घटित हुआ है। योग से सम्बद्ध इस विचारशील गूढ़ीकरण (दुर्बोधता) की ओट में कुछ स्वार्थपूर्ण उद्देश्य निहित हैं। इस सत्य विज्ञान की मिथ्या अभिव्यक्ति ने बहुत भ्रान्ति को जन्म दिया है। स्पष्ट और निःसंकुचित शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि वह सब जिसे हिन्दुओं ने योग की उपाधि प्रदान की है, वस्तुतः योग नहीं है। योग जादू नहीं है और न ही यह किसी असामान्य विलक्षण क्रिया का अनुष्ठान ही है।
योग फकीरी नहीं है जैसा कि पूर्व के अनेक यात्रियों और आगन्तुकों का मत है-विशेषकर संवाददाताओं का ऐसा मत है जो सामान्य और भावुक जनता को सदा विलक्षण और मर्मस्पर्शी समाचारों से चकाचौंध करते हैं। ये लोग पश्चिम में ऐसे मत-प्रसारण में सफल हो गये हैं कि किसी प्रकार से शरीर को कष्ट पहुँचाना ही योग है। जैसे कीलों की शय्या पर शयन, स्वयं को भूगर्भ में दबाना, काँच के टुकड़ों को चबाना और निगलना, ऐसिड पीना, कील निगलना अथवा पिन या सूचिका से स्वयं को बेधना। भारत के योगी का वे लोग ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर सकते हैं जिसने जटायें रखी हों, निर्वस्त्र कीलों की शय्या पर शयन करता हो अथवा जो कदाचित् किसी वृक्ष की शाखा से अधोशिर, पैर ऊपर करके लटका दिया गया हो। इसका योग से कोई सम्बन्ध नहीं और सच्चे योगी को इन सबसे कोई अभिप्राय नहीं है।
योग कोई संस्कार-विधि अथवा अनुष्ठान-विशेष नहीं है। यह भोगपरायणता नहीं है। यह प्रतिमापूजन (देवार्चना) नहीं है। यह सामुद्रिक विद्या नहीं है। यह भाव बताना नहीं है। यह भविष्यद्वाद (भाविकथन) नहीं है। यह विचार अध्ययन नहीं है और न ही यह भूत-प्रेत आदि के निराकरण हेतु मन्त्र-गान ही है। इनमें से कुछ भी योग नहीं है। यदि लोग स्वयं को योगी कह उन्हीं वस्तुओं की व्याख्या द्वारा अपना योग प्रदर्शन करें तो वे 'योग' शब्द का अप्रयोग कर रहे हैं। योग आपकी दिव्य प्रकृति के साक्षात्कार का शुद्ध विज्ञान है, अन्वयागत पूर्णत्व के उन्मीलन का पवित्र विज्ञान है, जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति का पवित्र विज्ञान है। योग सकृत्रिम निद्रा नहीं है। पुनः-पुनः मन्त्रोच्चारण अथवा समरूपेण अभिनय-विशेष के द्वारा सुषुप्तिजनक समाधि मैं उतरना नहीं है, यद्यपि तथाकथित प्रबुद्ध एवं मेधावी जनों का मत है कि जिन्होंने इस विज्ञान का अध्ययन किया है। ऐसी विचारधारा योग के वास्तविक महत्त्व के अवबोध का शत्रुतापूर्ण शोचनीय अभाव है।
लसर्जिक एसिड अथवा मैस्कलिन अथवा मैस्कलिन पेयोत अथवा दिव्य छत्र से प्राप्त अनुभवों के समान नहीं है। यह अनुभव योग नहीं है और न ही योगाभ्यास से प्राप्त होने वाले अनुभवों के समान ही है।
योग चमत्कारिक क्रिया अथवा रहस्य-व्यापार नहीं है, यद्यपि किंचित् यौगिक विधियाँ गुप्त रखी गयी हैं; किन्तु इसका एक सुन्दर और प्रत्यक्ष कारण है। जिस प्रकार से आप शिशु को किसी मशीन के दुर्बोध पुर्जे से दूर रखते हैं, जिस प्रकार आप यन्त्र के दुर्बोध पुर्जे को शिशु की पहुँच से दूर रखते हैं उसी प्रकार कुछ यौगिक कलाएँ भी गुप्त रखी गयी हैं; किन्तु यह रहस्य बनाये रखने के लिए नहीं है। यह तो मात्र उन लोगों से दूर रखने के लिए है जो इस विज्ञान के उन पक्षों में उतरने योग्य नहीं हैं, जिन्हें सावधानी और गहन ध्यान की आवश्यकता है। जब यही लोग अनिवार्य योग्यता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें अचिरेण ही गुप्त विधियों का आभ्यन्तर ज्ञान कराया जाता है। एवंविध योग रहस्य-व्यापार अथवा रहस्य नहीं है।
अन्ततः, योग धार्मिक सम्प्रदाय नहीं है। योग का उद्भव पूर्व में होने के कारण इसमें कतिपय पूर्वीय विचारधाराएँ निहित हैं। यह सत्य है; किन्तु ये विचारधाराएँ यथार्थ योग की केवल आध्यात्मिक भूमिका ही हैं। वास्तविक योग-विज्ञान के उद्भव से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। योग की व्यावहारिक और प्रभावशाली विधियों का अनुष्ठान सभी जातियाँ, राष्ट्र, सम्प्रदाय, मत, धर्म और गण कर सकते हैं। आपके सम्बन्धों का यहाँ कोई महत्त्व नहीं; क्योंकि व्यावहारिक क्रियाओं का यह शरीर पृष्ठभूमि में स्थित सभी आध्यात्मिक विचारधाराओं से सर्वथा पृथक् एवं भिन्न है। यह सत्य है कि हिन्दुओं द्वारा धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कतिपय विशेष विचारों का संशोधन करने के फलस्वरूप योग की प्रतिपत्ति हुई; किन्तु उनके अन्वेषणों का प्रतिफल योग सार्वभौम मूल्य रखता है। इस प्रकार से आपको 'योग' का आध्यात्मिकता से, जिससे इसका उद्भव है, स्पष्ट रूप से भेद जान लेना चाहिए। यह विचारधारा तो विशेष रूप से पूर्वीय और भारतीय है, किन्तु योग जो अपनी दार्शनिक और ऐतिहासिक पार्श्वभूमि से पृथक् किया जा सकता है, सैद्धान्तिक विचारों से परे है; इसलिए इसे यथार्थ रूप से हिन्दू-धर्म से सम्बद्ध नहीं मान सकते।
शोक, दुःख और पीड़ा-योग की उत्पत्ति
आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि योग कलाबाजी नहीं; जादू, संताप, संस्कार-विधि अथवा अनुष्ठान नहीं; भोगपरायणता अथवा प्रतिमापूजन नहीं; चमत्कार-क्रिया अथवा रहस्योन्मीलन नहीं; कृत्रिम निद्रा अथवा लसर्तुक ऐसिड अथवा मस्कलिन का अनुभव नहीं है। अब मैं योग का विवेचन करूँगा-योग क्या है : सारतः योग आध्यात्मिक विधि से सम्बद्ध आध्यात्मिक तत्त्व है। आपके जीवन के केन्द्र ब्रह्म-परम सत्य के साक्षात्कार हेतु यह अत्यन्त व्यावहारिक विधि है। योग मानवता का स्वाधिकार है।
संक्षेप में अब योग के उद्भव का विवरण दिया जायेगा। पृथ्वी पर मानव के जीवन का निरूपण करते हुए आपको स्वीकार करना होगा कि जीवन कार में बैठ-बैठे केवल आइसक्रीम, चाकलेट, मिल्क शेक ग्रहण करने का क्रीड़ा-स्थल नहीं है। यह जन्म, संवर्धन, पीड़ा, दुःखानुभूति, दुःख, हानि और लाभ है। मान-अपमान, आशा और निराशा, संघर्ष, क्लेश, व्याधि और अन्ततः मानव स्वरूप का क्षय तथा देहान्त है। ये प्रक्रिया अत्यन्त निष्ठुर एवं अपरिहार्य है।
मनुष्य दोषों एवं दुर्बलताओं का पुतला है। इच्छा-अनिच्छा सदैव उसके मन में वास करती है। किसी को तो वह अत्यन्त आत्मीय मानता है, अन्य जनों को वह अपना नहीं मानता और इस प्रकार से एक समुदाय की रुचि दूसरे समुदाय से विपरीत होती है। शत्रुता, विद्वेष और मात्सर्य भाव जागृत होते हैं। परस्पर घर्षण, संक्षोभ और विवाद प्रारम्भ हो उठते हैं। दुःख, क्लेश, व्याधि और निराशा, अपक्षय, विलय और मृत्यु आदि की बृहत् समस्या के कारण योग के उत्कृष्ट विज्ञान का उद्भव हुआ। सर्व रोगों एवं सर्व कालों के लिए योग अचूक और प्रभावशाली साधन प्रस्तुत करता है।
मनुष्य को जब दुःख और क्लेशों से छुटकारा पाने और सीमित अस्तित्व के कारण आवागमन के बन्धन से मुक्त होने तथा सब प्रकार के भय और मृत्यु पर विजयी होने की आवश्यकता अनुभव हुई तो फलस्वरूप 'योग' का उद्भव हुआ। इस महती समस्या का सुझाव योग का व्यावहारिक अभ्यास है। यह व्यष्टि पिण्ड और समष्टि पिण्ड के मध्य लुप्त सन्धि का संयोग करता है। योग स्पष्ट रूप से उपदेश देता है कि मनुष्य मूलतः आनन्द, सम्पूर्ण, शान्त और स्वच्छन्द प्रकृति का है। शाश्वत रूप से वह 'उसके' साथ एक है। उसकी सर्व सम्पन्न असीम परमात्मा के साथ अभेद भाव की जागृति का अभाव ही जीवन-रूपी इस भौतिक प्रक्रम में समावेश का कारण है।
वास्तविक जागृति की पुनर्प्राप्ति और दिव्यात्मा के साथ शाश्वत संयोग का पुनः बोध ही वस्तुतः योग का अभ्यास है। यह भौतिक संसार के दोष एवं अपूर्णताओं का अतिक्रमण करके स्व-स्वरूप में आत्म-स्थिति का अनुभव कराने का साधन है। योग निम्न प्रकृति की अपूर्णताओं का निराकरण करने एवं मन और इन्द्रियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पथ-प्रदर्शक है। मनुष्य नित्यतः सर्व सम्पूर्ण है। वह मन तथा इन्द्रिय नहीं है। मनुष्य वासनाओं से पूर्ण इन्द्रियों का उद्वेग नहीं है। वह इतस्ततः भटकने वाला, शताधिक विचारों से विशीर्ण कामना-युक्त मन नहीं है। सारतः वह दिव्य तत्त्व से उद्भूत सर्वांगीण सत्ता है।
व्यावहारिक अनुभव पर आधारित विज्ञान
सार रूप में मनुष्य दिव्यत्व से भिन्न नहीं है। मनुष्य की भी वही प्रकृति है और योगाभ्यास द्वारा वह उस दिव्य प्रकृति की जागृति पुनः प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। कतिपय विशेष यौगिक क्रियाओं के अभ्यास द्वारा मनुष्य ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर भौतिक स्तर से ऊपर उठ कर विशाल सर्वातिशायी आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचता है। यह उच्च स्तर ईश्वर-चैतन्य से एक हो जाता है। यह दिव्य चेतना है। ईश्वर-चैतन्य जगत्सम्बन्धी चैतन्य है। इस गरिमामय अनुभव में पराकाष्ठा को प्राप्त विविध व्यावहारिक क्रियाओं को शत-सहस्र बार पुनः पुनः अभ्यास करने वाले योगियों पर इस उपलब्धि की वृष्टि हुई है। शताब्दियों पर्यन्त ऋषियों और तत्त्वज्ञानियों ने इन क्रियाओं की अन्तिम चरण तक प्रामाणिकता सिद्ध की है। यह विज्ञान मात्र विश्वास पर ही नहीं, प्रत्युत इसके नियमों के व्यावहारिक अनुष्ठान द्वारा प्राप्त अनुभव पर निर्भर है। पारंगत योगियों ने वास्तविक साक्षात् अनुभव प्राप्त किया और गौरवपूर्ण अनुभव की सप्रमाण घोषणा की। ऐसे आचार्य आज के भारत के सर्व प्रदेशों में विद्यमान हैं।
भारत से बाहर भी पारंगत नर-नारी हैं जिनकी आत्माएँ इस दिव्यानुभव से प्रकाशित हुई हैं। किन्तु जीवन के उद्देश्य के प्रति भारत की विचारधारा इसी अनुभूति अर्थात् भगवद्-साक्षात्कार की ओर इंगित करती है। इसलिए भारत से बाहर भगवज्योति से प्रकाशित आत्माएँ अपेक्षाकृत कम हैं। संख्या में अल्प हों; किन्तु अमेरिका, यूरोप और सुदूर पूर्व में उच्छृत (high) आध्यात्मिकानुभूतियों से युक्त महात्मा विद्यमान हैं। अभिज्ञान की आकांक्षा न करते हुए वे प्रायः अज्ञातवास करते हैं। वे सब योगी ही हैं। आप उनके अभ्यास पर 'योग' की परिभाषा को लागू करें अथवा नहीं, उनके जीवन का ढंग, उनकी उपलब्धि 'योग' शब्द की संस्कृत परिभाषा के अनुसार यौगिक है अर्थात् दिव्यात्मा के साथ एकता की अवस्था अथवा महान् सत्य (परमात्मा) के साथ अभेद भाव की अनुभूति। यह योग का यथार्थ अभिप्राय है। योग का अर्थ है-सत्यानुभूति अथवा वास्तविकता का बोध अथवा दिव्य तत्त्व के साथ संयोग।
योग शब्द के गौण अर्थ भी हैं। अन्ततः अभ्यासी को दिव्य बोध प्रदान करने वाले सभी साधन एक शब्द 'योग' की उपाधि से आख्यात हैं। ये विविध साधन एक शब्द 'योग' की उपाधि से आख्यात हैं। ये विविध प्रक्रियाएँ स्पष्ट वर्गीकरण हेतु चार विभिन्न व्यावहारिक उपगमनों में विभाजित कर दी गयी हैं जिनमें से प्रत्येक उस एक महान् सत्य की अनुभूतियों में पराकाष्ठा को प्राप्त है। विशेष निश्चित, वैज्ञानिक ढंग से उत्पन्न और बुद्धिमत्तापूर्वक विरचित प्रक्रियाएँ मनुष्य को, उस के शरीर, मन और इन्द्रियों की प्रकृति द्वारा अध्यासित सर्व दोषों का निराकरण करने और अपने विचारों को सर्वथा परमात्मा पर एकाग्र करने के योग्य बनाती है। इस परिभाषा के अनुसार योग का अर्थ है-मन को ईश्वरोन्मुख करना, दिव्य तत्त्व की आभ्यन्तर उपासना के गूढ़ स्तर पर पहुँचना और अन्ततः दिव्य चेतना के साथ अभेद भाव का अवबोध करना। अतः 'योग' शब्द की सरल परिभाषा के अनुसार कोई भी प्रयत्न जो आत्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हेतु किया गया हो, 'योग' है।
यह कोई भी वस्तु हो सकती है जो आपने योग-सम्बन्धी पुस्तकों में देखी हो अथवा कोई भी क्रिया जो आपने बिना किसी बाह्य प्रेरणा के करनी प्रारम्भ की हो। यदि आपको आभास होता कि अमुक वस्तु-विशेष आपको ब्रह्म की ओर उन्मुख करने में सहायता करती है और आपके व्यक्तिगत स्वभाव तथा आवश्यकता के अनुकूल है, तो वह वस्तु आपके योग का अंग है। वह किसी योग की पुस्तक में उपलब्ध हो अथवा नहीं और किसी हिन्दू आचार्य ने आपको उसका निरूपण दिया हो या नहीं, योग में विस्तार का स्थान है। यह ऐसा कठोर विज्ञान नहीं है जिसमें परिवर्तन और समाधान निषिद्ध हों। मौलिक साधन सारतः अपरिवर्तित रहते हैं; किन्तु क्रियाएँ अभ्यासकर्ता के अनुकूल परिणत हो सकती हैं जो पूर्वीय पाश्चात्य अथवा स्त्री एवं पुरुष पर निर्भर हैं। और भी एक विधि विशेष रूप में एक विशेष अवस्था अथवा काल में आपके आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल हो सकती है; किन्तु वही आपके आध्यात्मिक जीवन की अन्य अवस्था में परिवर्तित हो सकती है।
इस स्वरूप-भेद योग के दर्शन एक सरलतम रूप में किये जा सकते हैं। यह है-दिव्य नाम-जप का अभ्यास । भगवन्नाम के निरन्तर जप द्वारा आप भगवद्-विचार सदा मन में धारण किये रहते हैं। उसके इस प्रकार के स्मरण से आपको उसकी विद्यमानता का आभास होने लगता है और इससे आपका मन अन्य अयुक्त विचारों से मुक्त रहता है। आप मन को शान्ति और स्थैर्य में परिस्थापित करके एकान्त में आन्तरिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
भगवन्नाम का जप कर्णगोचर रूप से अर्थात् उच्च स्वर में करना चाहिए। यदि आप अपनी ध्वनि स्वयं श्रवण करें, तो मन एकाग्रचित्त हो जाता है। तदनन्तर, जैसे-जैसे आप उन्नति करते हैं और आपमें मन को सतत एकाग्र करने की क्षमता आने लगती है, आप श्राव्य जप छोड़ कर निःशब्द मानसिक जप प्रारम्भ कर सकते हैं। एवंविध, दिव्य नाम-जप की एक ही विधि आप प्रथमतः प्रारम्भ करते हैं और उत्तरकाल में स्व-चैतन्य और अनुकूलता के स्तर के आधार पर इसे विधि-विशेष में रूपान्तरित करते हैं।
अन्तर्निहित अधिकृत दिव्य पूर्णता के उन्मीलन हेतु योग एक सक्रिय साधन है। आप नाम-रूप से भिन्न आत्म-तत्त्व हैं। मन तो आपकी अभिव्यक्ति हेतु मात्र माध्यम है। योग आपको सत्य प्रकृति की जागृति की ओर अग्रसर करता है। योग के द्वारा आप परमात्मा के साथ शाश्वत अभिन्न रूप से साक्षात्कार हेतु योग्यता ग्रहण करते हैं।
सर्वकाल में सार्वभौमिक नियम
इस विज्ञान के उद्भव के समय महर्षि हिन्दू अथवा पूर्वीय आदि, गण-विशेष की आवश्यकताओं से अधिक सम्बद्ध न थे, अपितु उन्होंने धरती पर मनुष्य को उसकी वास्तविक संरचना के रूप में जानना स्वीकार किया। उन्हें यह स्पष्ट ज्ञान था कि भौतिक शरीर और मन विशेष कार्यों का प्रतिपादन करते हैं। शरीर मन का एक साधन है और मन आत्माभिव्यक्ति का स्रोत है। उन्होंने अवेक्षणा की कि अत्यन्त दुर्भाग्यवश मनुष्य शरीर का दास बन कर इन्द्रियों के इन्द्रजाल में फँसा और मन की तृष्णाओं का शिकार बन कर पीड़ाग्रस्त हुआ। यह थी पार्थिव मनुष्य की दशा-इन्द्रियों का दास और तृष्णाओं से बँधा हुआ, जिसके आत्म-तत्त्व का तेज पूर्णतया कलंकित हो चुका था-योगाभ्यास द्वारा इस दशा को सुधारने की उन्हें आकांक्षा हुई।
योग में साधन है जिसके द्वारा आप इन्द्रियों को वशीभूत करके, मन पर प्रभुत्व पा कर, इच्छाओं और विचारों को अतिक्रमण द्वारा संयत करके शरीर-बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने अस्तित्व की अन्तस्तम गहराई को पहुँचते हैं, जहाँ आपको ज्ञात होता है कि आप वस्तुतः किस लिए आये हैं; एक सम्पूर्ण एवं दिव्य सत्ता। योग किसी स्थान अथवा धर्म-विशेष के मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया। जब जनता मुझसे आधुनिक मन के लिए योग की अनुकूलता का प्रश्न करती है, तो मैं अनुभव करता हूँ कि प्रश्न निरर्थक है; क्योंकि योग के सम्बन्ध में आधुनिक मन-रूपी कोई विषय नहीं है। योग का सम्बन्ध नित्य मनुष्य के साथ है। यह आपके मन और स्थूल तत्त्व के अन्तर्निहित दिव्य सत्त्व से सम्बद्ध है; क्योंकि इसका अस्तित्व सृष्टि के आदिकाल से है और सृष्टि के विलय पर्यन्त रहेगा। इसमें प्राचीन और अर्वाचीन का कोई प्रश्न ही नहीं है; अतः आप स्वयं को अभी अर्वाचीन कह सकते हैं, किन्तु दो सहस्र वर्षोपरान्त लोग सन् १९०० पर दृष्टिपात करेंगे और कहेंगे- "अहा! विगत युग के वे प्राचीन पुरुष!" अतः आधुनिक तो मात्र सापेक्षिक व्याख्या है, जब कि योग न केवल गत, प्रत्युत वर्तमान और सुदूर भविष्य का भी विज्ञान है। यावत्पर्यन्त पृथ्वी पर मानव-सत्ता है, तावत्पर्यन्त वह पीड़ा, दुःख, व्याधि, जन्म, मृत्यु के बन्धन से मुक्त न होगा और योग ही सदा इस समस्या का समाधान होगा।
योग का प्रयोजन सार्वभौम है। धार्मिक जीवन के स्वरूप के अन्तर्गत इसका अनुष्ठान किया जा सकता है; किन्तु यह धर्मातीत है, यह परम धर्म है। योग किसी भी सिद्धान्त अथवा मत से परे है। जहाँ तक इसके विचारों का सम्बन्ध है, इसका आधार समस्तरूपेण सार्वभौम है। इसके अनुष्ठान का विस्तार सम्पूर्ण मानवता के साथ सर्वकाल के लिए सम्बद्ध है।
अब जैसा कि हमें ज्ञात है कि जीवन की प्रमुख समस्या मनुष्य का मन और प्रकृति के साथ बन्धन है, इसमें वस्तुतः योग किस प्रकार से सहायता करता है?
संक्षेप में, यह आपको बन्धन-मुक्त कराने का यत्न करता है और एक बार पुनः आपको अपनी शाश्वत दिव्य प्रकृति की पुनः जागृति कराता है। योगियों ने अनुभव किया कि सबसे बड़ी बाधा और रुकावट मन का वह विचार है जिसमें आप कहते हैं—“मैं यह शरीर हूँ, यह ससीम मनुष्य हूँ। दुःख-पीड़ा मेरा धर्म है। मैं अमुक-अमुक वस्तु से सम्बद्ध हूँ। मुझे अमुक वस्त्र की आवश्यकता है। मुझे बुभुक्षा और तृषा लगी है।" सुख प्राप्त करने और दुःख-निवारण के लिए मन मनुष्य को अपने इस स्वरूप से सतत एकात्मक रखता है जो अनित्य है। मन सर्वशः बहिर्मुख हो जाता है। यह इन्द्रियों के द्वारा ऐन्द्रिक-विषयों की ओर जाता है। यह केवल बाह्य विश्व का अवलोकन करता है। यह संहरण द्वारा इन्द्रियों से विमुख हो कर अपनी आभ्यन्तरिक गहन प्रकृति की अवेक्षणा नहीं करता है जो यथार्थ और अन्तस्तम है।
मन बाधा है। मन की बाह्य गति का मार्ग इन्द्रियों में खोजा जा सकता है। अन्ततोगत्वा, मन ही परम इन्द्रिय और प्रमुख साधन है। इस समय यह बाह्य विषयों में बँधा हुआ है। अवधानपूर्ण अन्तर्दृष्टि द्वारा यदि आप इसे अन्तर्मुख कर लें, तो अपनी मानव-प्रकृति के सर्व दोषों और दुर्बलताओं का अतिक्रमण करने में समर्थ हो जायेंगे जो आपकी दिव्य प्रकृति में स्थित आनन्द और प्रशान्ति के अनुभव को अपहृत किये हुए हैं।
योग में मन का प्रशिक्षण
मन की चतुर्विध अभिव्यक्ति है। प्रथमाभिव्यक्ति है विवेक-शक्ति, द्वितीय प्रेम अथवा भावाभिव्यक्ति, तृतीय सक्रियता एवं चतुर्थ, प्रतिबिम्ब अथवा ध्यानपरता। मन की इन चारों अभिव्यक्तियों को अन्तर्मुख करने के लिए प्रशिक्षित और संयत करना है जिससे आपके साधन पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जायें और महान् लक्ष्य शुद्ध चेतन की ओर उन्मुख हों।
तर्क-शक्ति विश्व के सुदूर स्थलों में प्रकीर्ण नहीं करनी चाहिए। यह शक्ति आपके भीतर उस परम तत्त्व का बोध कराने वाली हो जो अन्तर्निहित है और सब ज्ञान का स्रोत है, प्रकाश है जो आपकी ही बुद्धि को प्रकाशित करने वाला है। इसके बिना आप न सोच सकते हैं, न ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। योग में अनन्त विधियाँ बतायी गयी हैं जिनके द्वारा वृत्तियों को परम सत्य की ओर, सर्वभावों को परब्रह्म की ओर, आपकी सम्पूर्ण शक्ति को महान् लक्ष्य की ओर, विवेक-शक्ति को आत्यन्तिक सत्य परमात्मा की ओर उन्मुख किया जा सकता है। मन और प्रकृति की इस चतुर्विध अभिव्यक्ति की अद्वितीय परम लक्ष्य की ओर उन्मुखता आपको शोकातीत अवस्था की ओर अग्रसर करके सदा-सदा के लिए मन और इन्द्रियों के बन्धन-रूपी दासता से मुक्ति प्रदान करती है तथा आप पर आत्म-साक्षात्कार के तेजस्वी अनुभव की वृष्टि करती है। आप अमर हो जाते हैं।
योग मन को परब्रह्म में लीन करने का विज्ञान है। आप अपना समस्त प्रेम अपने अस्तित्व के परम स्रोत की ओर प्रवाहित करने लगते हैं। अपनी समस्त क्रियाएँ महान् लक्ष्य, परम धाम को समर्पण करने लगते हैं। आप अपने समग्र विचारों को इस प्रकार से एकाग्र करते हैं कि वे इस नानाविध ब्रह्माण्ड से संहत हो कर परमात्मा के उस महान् और गौरवान्वित विचार में लीन हो जाते हैं।
समस्त विवेकपूर्ण योग्यताओं को भगवद्-साक्षात्कार में उन्मुख करना ज्ञानयोग कहलाता है। योग के इस अंग में विवेकपूर्ण सत्यता को ग्रहण करने के प्रयास में मनुष्य वास्तविक ज्ञान-शक्ति द्वारा एक उत्कृष्ट क्रिया का अभ्यास करता है। भगवद्-प्रेम में पूर्ण क्षमता का विकास भक्तियोग अथवा प्रेमयोग कहलाता है। जीवन के सर्वकर्म परमात्मा को समर्पित भाव से करना भी एक योग-प्रणाली है जिसमें आप अपने जीवन की क्रियाओं के विविध पक्षों का निःस्वार्थ भाव से समीकरण करते हैं। अन्ततः राजयोग में मनुष्य को अपनी सत्ता के केन्द्रिय बिन्दु परब्रह्म के प्रति अधिकाधिक सचेत करके अत्यन्त विशेष प्रक्रिया में प्रवृत्त किया जाता है जिससे उसका चित्त पूर्णतया परब्रह्म में लीन हो जाता है। अनेक हृदयग्राही लक्षण दृष्टिगत हुए हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि अनेक पाश्चात्य साधक अपनी सभ्यता की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु योग की इस प्रणाली के विषय में सर्वाधिक अनुकूल साधन के रूप में प्रयोग करने का गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।
अब आपको योग और आत्मा के मध्य का सम्बन्ध स्पष्ट हो गया है। योग आपको भगवद्-प्राप्ति के वैज्ञानिक साधन उपलब्ध कराता है। वस्तुतः इस पहुँच में जो-कुछ भी करते हैं, वह योग ही है, भले ही उसे इस स्वरूप में लक्षित किया गया हो अथवा नहीं। इस व्याख्या में एक अत्यन्त आश्चर्यजनक अनुमान उठता है कि फिर तो सभी ईसाई सन्त और रहस्यवादी जिन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवद्-प्रेम तथा उपासना करने का प्रयास किया है और उस पर ध्यानस्थ हो कर आत्मैक्य प्राप्त किया है, योगी होंगे। सन्त 'जौन' एक महान् भक्तियोगी और ज्ञानयोगी था। क्रास (Cross) के सन्त जौन और अविला (Avila) के सन्त तेरसा, दोनों महान् राजयोगी थे। वे ध्यान के रहस्यवादी थे जिन्होंने एकाग्रता और ध्यान द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त किया।
यदि इन सबने योग का ही अनुसरण किया है, तो भारत में अनुष्ठित योग की विशेषता और लक्षण क्या है?
भारत के सन्तों का आध्यात्मिक अन्वेषण
प्रथमतः, योग की असामान्यता के सम्बन्ध में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका भारत में अभ्यास किया जाता हो। अन्य स्थानों में की जाने वाली विधियों का यहाँ भी अभ्यास किया जाता है। पुनरपि, जहाँ तक योग की विशिष्टता का प्रश्न है, वह यह है कि एकाग्रता और ध्यान की प्रक्रियाओं का स्पष्ट मत भारत में ही प्राप्त हो सकता है। भारत के ऋषियों ने ज्ञान की प्राप्ति हेतु गहन और विस्तृत आध्यात्मिक खोज की, जो मनुष्य को निम्नावस्था से आत्यन्तिक तेजपूर्ण अवस्था की ओर ले जाती है जो उसे उपलब्ध करना है। उन्होंने इतने विस्तार में इस प्रक्रिया का अध्ययन करने का प्रयास किया कि दिव्यारोहण पथ में शरीर-विच्छेद-विद्या-शास्त्र (anatomy) की पूर्ण अभिव्यक्ति हो गयी। प्रत्येक अंग का पूर्णतया विश्लेषण और ज्ञान हो गया। अध्ययन से उन्होंने जाना कि अभ्यासी साधक के पथ में कौन-कौन-से विघ्न आते हैं। उन्होंने खोज की कि ये विघ्न क्यों आये और मनुष्य-प्रकृति में कौन-से ऐसे तत्त्व निहित थे जो इन बाधाओं के मूल कारण थे। इन विघ्नों के मूलतः निराकरण हेतु उन्होंने साधन ढूँढ़ा। इस कार्य हेतु उन्होंने अद्भुत कल्पनाओं का अनुष्ठान किया, अभ्यास किया और उन्हें प्रभावशाली प्रमाणित किया। इन प्रक्रियाओं की कार्यवधि एवं अनुष्ठान के सम्बन्ध में उन्होंने उपदेश दिया। आन्तरिक यन्त्र रचना का उनका ज्ञान अद्भुत था। मानव-संरचना के प्रति उनका ज्ञान अद्वितीय था। भारत के योग की यही विशिष्टता है।
एक हृदय-रोग विशेषज्ञ को हृदय रोग विशेषज्ञ और मस्तिष्क-रोग विशेषज्ञ को मस्तिष्क-रोग-विशेषज्ञ कहते हैं। ये विशेषज्ञ स्व-स्व विज्ञान में इतना गहन उतर गये हैं कि उन्होंने अपने अध्ययन में सर्व उपलब्ध तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से मानव-प्रकृति में रूपान्तरण आध्यात्मीकरण तथा दिव्यत्त्व लाने की प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए भारतीय आचार्यों ने मानव-सत्ता की गहराई में गोता लगाना अपना जीवन-कार्य बना लिया। कोई भी विषय अस्पृष्ट नहीं रहा। मन, शरीर एवं इन्द्रियों तथा इन पर प्रभुत्व करने वाली विविध शक्तियों जैसे भोजन जो आप भक्षण करते हैं, संगति एवं आचार-व्यवहार जिसका आप विकास करते हैं-इन सबका उन्हें पूर्ण ज्ञान था। अतएव, योग में विज्ञान का विकास पूर्णत्व की इस पराकाष्ठा को पहुँचा कि इसमें हमें विवेक तथा व्यावहारिक ज्ञान का सार प्राप्त होता है जो मनुष्य ने शताब्दियों पर्यन्त (तपस्या के पश्चात्) उपलब्ध किया। अन्य जनों ने इतस्ततः इस ज्ञान को अंश-रूप में धारण किया; किन्तु योग में यह पूर्ण एवं सिद्ध है। योग के द्वारा यह परिनिष्पन्न ज्ञान सम्पूर्ण मानवता को प्रदान किया गया है।
यौगिक जीवन का सार्वभौम स्वरूप
अब यौगिक जीवन के सार्वभौम स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया जायेगा। सर्वप्रथम योग जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध करना है, यह आपको इस प्रश्न का उत्तर देता है- "मैं यहाँ क्यों आया हूँ और जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है?" ब्रह्माण्ड की यथार्थ प्रकृति के प्रति योग द्वारा आपको ज्ञान होने पर आप जान जाते हैं कि नश्वर और क्षणभंगुर गमनशील पदार्थों के मोह में आसक्त नहीं होना है। इन्द्रिय विषय, सुख और आनन्द का, दोष रहित अनुभव नहीं प्रदान करते। योग से विषयों के वास्तविक स्वरूप की प्रतीति होती है, दृश्यमात्र स्वरूप की नहीं। यह आपको सावधान करता है कि विषयों की बाह्य चमक-दमक की भ्रान्ति में नहीं पड़ना, उनसे धोखा नहीं खाना और इस प्रकार उनके प्रलोभन 7/4 फँस कर उनकी दासता नहीं करना। योग आपको विरक्ति का आदेश देता है; क्योंकि यदि विषयों में आप आसक्त हैं, तो आपको फलस्वरूप दुःख ही भोगना पड़ेगा।
अविनाशी सत्य परमात्मा ही सर्व सम्पूर्ण है जिसकी प्रकृति परमानन्दमय तथा अप्रमेय शान्ति की है। आपमें अन्तर्निहित सच्चे सुख की प्यास, सर्वबन्धनों से सच्चे मोक्ष, सब प्रकार के भय तथा मृत्यु-क्रम से भी मुक्ति की तृषा केवल वही शान्त कर सकता है। योग आपका लक्ष्य-निर्देशन करके इसकी प्राप्ति की प्रगाढ़ प्रेरणा को विकसित करने का उपदेश देता है। एक स्तिमित प्रशान्त और सन्तुलित जीव बन कर, विषयों के आकर्षण से अप्रभावित रह कर जीवन में कैसे संघर्ष करना है- योग इसका निर्देशन करता है। इसके अनुसार विषयों की शक्ति से अनायास ही असन्तुलित हो कर दास की भाँति उद्विग्न और भयग्रस्त नहीं होना है।
एवंविध जीवन में अनासक्त शान्तिपूर्वक चलने के लिए मनुष्य सन्नद्ध हो जाता है और यदि किसी प्रकार की आसक्ति हो तो वह परम पिता परमात्मा के साथ ही होती है, जीवन की विधा जो ईश्वर की ओर ले जाती है, उससे होती है। ये आसक्ति आपकी निम्न प्रकृति को परिशुद्ध करती है। चेतन का विस्तार करके आपको दिव्य सत्ता की जागृति के निकट ले आती है। प्रभु से आसक्ति करो। भौतिक एवं नश्वर पदार्थों से आसक्ति-रूपी दुःखद भूल का त्याग करो। वैराग्य और विवेक विकसित करो जिनसे सब विषयों का उनके वास्तविक रूप में ज्ञान हो जाता है। तीव्र जिज्ञासा को जागृत करो।
ये प्रक्रियाएँ यौगिक जीवन में यथार्थ उन्मीलन की ओर अग्रसर करती हैं। योग-विज्ञान मनुष्य का ही अध्ययन करके घोषणा करता है कि वह त्रिविध प्रकृति युक्त प्राणी है-प्रथमतः मनुष्य स्थूल एवं पाशविक प्रकृति से युक्त, द्वितीयतः विवेकशील किन्तु अशुद्धताओं एवं असंख्य सन्देह युक्त प्रवृत्तियों से पूर्ण और तृतीयतः दिव्य प्रकृति युक्त जो गहन अन्तरात्मा में स्थित है, सर्वशुद्ध और सर्वशक्तिमान है। आप दोष रहित पूर्णत्व से युक्त हैं। इसी सारतत्त्व में प्रशान्ति, आनन्द, स्वाधीनता, ज्योति और ज्ञान निहित है।
जीवन के यौगिक स्वरूप का सर्वप्रथम अंग है-निम्न प्रकृति की शुद्धि। शरीर-मन प्रकृति की अनेक अशुद्धताएँ मनुष्य की वास्तविक शत्रु हैं। उसके शत्रु का निवास बाहर नहीं है। भय एटम बम और मशीनगन से नहीं है। वास्तविक शत्रु तो हैं भौतिक वासनाएँ, क्रोध, लोभ, मोह, दर्प और ईर्ष्या। ये मनुष्य के शत्रु हैं, मानव-प्रकृति की ये छह अशुद्धताएँ हैं।
विवेकपूर्ण प्रयास से इन अशुद्धताओं का पूर्णरूपेण अतिक्रमण किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता से मनुष्य अपनी आत्मा का स्वामी बन कर अन्तःस्थित सब उत्कृष्टतर गुणों, भद्रता और धर्म को उद्दीप्त कर सकता है। वह अशुद्धताओं से युक्त मात्र पाशविक प्राणी नहीं, प्रत्युत ब्रह्म-प्रकृति के गुणों से युक्त ज्योतिर्मय व्यक्तित्व है। दया, प्रेम, सत्य, शुद्धता, निःस्वार्थपरता आदि गुणों का आपने स्वयं में विकास करना है। इस अभ्यास से जीवन के सच्चे उद्देश्य का बोध होता है।
विविध यौगिक पद्धतियाँ
योग की विविध पद्धतियाँ हैं जिनका विवरण यहाँ अत्यन्त संक्षेप में दिया जायेगा। ज्ञानयोग में मनुष्य को सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा की प्रकृति की व्याख्या का श्रवण, पुनः-पुनः इस पर मनन, तर्क-शक्ति और बुद्धि तथा अन्ततः गहन ध्यान में इस पर चिन्तन द्वारा परमात्मा का बोध होता है। भक्तियोग में मनुष्य परमात्मा के प्रति अत्यन्त प्रिय, व्यक्तिगत विषय-अपने ही माता-पिता, प्रिय मित्र, गौरवशाली सम्राट् और श्रद्धेय, पूज्य, प्रिय स्वामी के रूप में स्पष्ट धारणा रखता है। तदुपरान्त एक सम्बन्ध जोड़ा जाता है जिससे पावन प्रेम और श्रद्धा उसकी ओर प्रवाहित की जाती है। यह सब मनुष्यों द्वारा स्व-स्वरूप में स्थापित किये गये सम्बन्धों पर आधारित हैं। कोई व्यक्ति उसे अपने पुत्र अथवा दुहितृ अथवा शिशु-रूप में मानता है। अन्य व्यक्ति स्वयं को पिता मान कर भगवान् को दिव्य शिशु के रूप में कदाचित् बालक ईसा के रूप में ग्रहण करता है। कोई स्वयं को भगवान् का विनीत सेवक मान कर उसकी सेवा में जीवन के सब कर्म समर्पित कर उससे प्रेम करता है। अन्यथा, मनुष्य भगवान् के स्वमित्र रूप में दर्शन करता है। यह मानवीय सम्बन्ध हैं जिनसे सब जन परिचित हैं। इसमें कोई ऐसी असामान्यता अथवा आश्चर्य नहीं है। एवंविध, परमात्मा की ओर प्रवृत्ति और प्रेम-प्रवाह विशिष्ट रूप में भाव-प्रधान व्यक्ति को अनुकूल होते हैं। यह अत्यन्त मधुर पथ है। सतत प्रभु-चिन्तन, प्रार्थना, उपासना और उसकी सन्निधि के अनुभव द्वारा मनुष्य सुगमतया इस प्रकार का इतना गाढ़ सम्बन्ध स्थापित कर लेता है कि वह स्वाभाविक रूपेण ही उस प्रभु के साथ गमन, सम्भाषण, सहवास, भ्रमण और निजात्मा में उसकी अनुभूति करने लगता है। इस प्रकार से वह पूर्णतया अखण्ड रूप हो जाता है। कर्मयोग में प्रमुख क्रिया अहंकार का विनाश है। विनय और निःस्वार्थपरता ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को दिव्य स्वरूप प्रभु के दर्शनार्थ साधन-स्वरूप तैयार करते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत अहंभाव का पूर्णरूपेण निराकरण अनिवार्य है, तभी सब भौतिक प्राणी प्रभु की साक्षात् अभिव्यक्ति-स्वरूप और मन्दिर-रूप दृष्टिगत होने लगते हैं जिसमें परमात्मा अधिष्ठित है। परोपकार मनुष्य का स्वाभाविक कर्म बन जाता है और इस प्रकार प्रत्येक कर्म लौकिक कर्म न रह कर पूजा कर्म में परिणत हो जाता है। प्रत्येक कर्म को दिव्य साक्षात्कार में रूपान्तरित करने में संलग्न रहने वाला व्यक्ति सर्वत्र पूजा करता है। विद्यालय में शिक्षक, चिकित्सालय में डाक्टर, क्षेत्र में कृषक, स्टाक ऐक्सचेंज में व्यापारी-सभी क्रियारत हो सकते हैं जो आन्तरिक भाव द्वारा उपासना में परिणत हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से व्यावहारिक प्रतीत होने वाले व्यावसायिक क्रिया-कलाप भी योगाभ्यास का साधन बन सकते हैं।
योग की चतुर्थ पद्धति है-(ध्यानयोग) एकाग्रता और ध्यान द्वारा वृत्तियों का समाहरण और उनको प्रभु में लीन करना। यह मार्ग भी अत्यन्त सुन्दर है। विचार मन की गति है। मन की गति, जीवन की शक्ति प्राण तथा देह की गतिविधि से प्रवाहित होती है। शरीर, आध्यात्मिक मस्तिष्क शक्ति एवं विचार-तीनों एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं। योग की इस उत्कृष्ट रूप से व्यवस्थित पद्धति में शारीरिक संयम तथा नियन्त्रण विहित है जो शरीर को स्थिर मुद्रा में रखने से प्राप्त होता है। प्राणायाम द्वारा अन्तर्निहित आध्यात्मिक शक्ति का निग्रह होता है। अन्ततोगत्वा प्रक्रिया की पराकाष्ठा में मन की भटकती वृत्तियों का संहरण करके उसे आत्म-चिन्तन में एकाग्र किया जाता है। एकाग्रता के लिए अनेक प्रक्रियाएँ वर्णित हैं जिनमें से प्रत्येक मनुष्य किसी अनुकूल प्रक्रिया का अभ्यास आरम्भ कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य मानसिक स्तर से ऊपर उठ कर परम चैतन्यावस्था में पहुँचता है जिसमें उस पर अभेद भगवद्-साक्षात्कार की अनुभूति रूपी वृष्टि होती है और वह आवागमन के बन्धन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से परामुक्ति प्राप्त हो जाती है।
शुचिता-सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आधारशिला
सभी यौगिक कलाओं में सम्पूर्ण नैतिक तथा धार्मिक शुद्धि अनिवार्य है। शुचिता यौगिक जीवन की नींव है। दुराचारी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अशुद्ध, अश्रद्धालु, असत्यवादी, कपटी और अपकारी हो कर इन अवगुणों के साथ योगाभ्यास नहीं कर सकता। आभ्यन्तर परिस्थितियाँ अपूर्ण होने पर आध्यात्मिक साक्षात्कार होना असम्भव है। जीव में जब तक धार्मिक गुणों का गहन निधान न हो, तब तक धर्मानुष्ठान अथवा सात्यिक अन्तर्मुख जीवन नहीं बन सकता। भद्रता, शुचिता, सत्य और निःस्वार्थ में अधिष्ठित होना अनिवार्य है। योग की आधी प्रक्रिया तो पूर्ण रूप से आदर्श नैतिक चरित्र का निर्माण करना है। नींव के पड़ जाने पर तो यौगिक नियमों का अनुष्ठान माचिस के ऊपर शुष्क शलाका के घर्षण के समान है-तत्काल ही अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। बिना इस आधार के तो ये अशुष्क शलाका साबुन की टिकिया पर रगड़ने के समान है जिसका परिणाम शून्य होगा।
यावत्पर्यन्त मनुष्य आसक्ति से शुद्धि, असत्य से सत्य, कठोरता और निष्ठुरता से दया में परिणत नहीं होता, तावत्पर्यन्त यौगिक जीवन का विचार उससे कोसों दूर है। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि जब तक मनुष्य धार्मिक और नैतिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं है, तब तक वह योगाभ्यास में प्रवेश ही नहीं पा सकता। योगाभ्यास हेतु ही मनुष्य का जन्म हुआ है। यही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अन्य सभी कर्म गौण हैं और उनका प्रमुख उद्देश्य इसी प्रमुख कर्म से है। अतएव, चरित्र सदाचारी हो अथवा न हो, मनुष्य को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यत्नशील रहना है।
आध्यात्मिक जीवन के प्रारम्भिक काल में मनुष्य को पूर्ण नैतिक भद्रता और नैतिक पवित्रता के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य की सिद्धि पर बल देना है। योग के अन्य सभी पक्षों का प्रारम्भ में द्वितीय स्थान है। तदुपरान्त जब यह कार्य सुचारु रूपेण निष्फल हो जाये, शुद्ध अन्तर्मुख जीवन पर अधिकाधिक बल देना है। महात्मा ईसा अत्यन्त सहज रूप से इस सत्य को घर ले आये। उन्होंने कहा- "जब आप मुझे अर्चना अर्पित करने के लिए वेदी के समीप आते हैं, तो सर्वप्रथम स्मरण करें कि यदि आपके किसी मित्र ने आपका अपमान किया हो और आपने उसे क्षमा न किया, तो अभी जायें और उसे क्षमा-दान दे कर आयें, अन्यथा आपकी अभ्यर्चना स्वीकार न होगी।" उन्होंने यह भी कहा- “यदि आप सात बार नहीं सत्तहत्तर बार भी अपमानित हुए हों, तो भी अपमानकर्ता को क्षमा करते जायें; क्योंकि यदि आपका हृदय मनुष्य के प्रति प्रेम से परिपूर्ण नहीं होगा, सब जीवों के साथ अभेद भाव न होगा, तो आप न तो भगवान् के पास पहुँच सकते हैं और न ही भगवद्-प्रेम प्राप्त कर सकते हैं।"
एवंविध 'देवालय' में प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति को समर्थ किया जाता है, परमात्मा स्वयं दयालु और प्रेमस्वरूप है और यदि मनुष्य उस प्रकृति में अपना विकास नहीं करता, तो उस प्रकृति के समीप पहुँचने में समर्थ कैसे होगा? दैविक बनने पर ही आप परमेश्वर को पायेंगे; तब भगवान् स्वयं आपकी सात्त्विक प्रकृति के साथ एकरूप हो जायेंगे। तब अपूर्ण मानवीय प्रकृति का कोई भी विघ्न आपके और ब्रह्म के मध्य बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। दिव्य जीवन का पोषण सर्वोच्च स्तरीय नैतिक और धार्मिक पूर्णत्व से होगा। आत्म-संयम और निग्रह द्वारा इसका विकास किया जायेगा और गहन और उग्र ध्यान द्वारा आत्यन्तिक रूपेण यह फलीभूत होगा।
यौगिक जीवन के सभी पक्षों में प्रमुख तत्त्व भगवद्-कृपा है। इसे आप स्वेच्छा से कोई भी उपाधि दे सकते हैं। यह परमात्मा की कृपा है जो सब प्राणियों का स्रोत है और केवल उसी में मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप तथा अविनाशी दिव्यत्व का बोध करता है। सभी प्रकार के अभ्यास उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं, जब वे मनुष्य को परब्रह्म की ओर प्रवृत्त करके उसमें लीन कर देते हैं।
एवंविध, संक्षेप में—अच्छे बनो, अच्छा करो, दयालु बनो, करुण रूप बनो; सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो, सबमें भगवद्-दर्शन करो; विनीत बनो, सरल बनो; पवित्र बनो, अनन्यमनस्क बनो, ध्यान करो, भगवद्-साक्षात्कार करो तथा परम आनन्द की प्राप्ति करो।
१४. ध्यान और प्रार्थना
हमारा सौभाग्य है कि हम ध्यान के महान् विषय पर अब विचार करने लगे हैं। यह ऐसा विषय है जो सृष्टि के उदय के साथ मानव के समक्ष आने वाली तथा मानव का आह्वान करने वाली जन्म-मृत्यु रूपी समस्या का आत्यन्तिक समाधान है।
ध्यान उस समस्या का समाधान है जो व्यक्ति को जीवन के प्रति कटुता तथा दुःख और क्लेश से आक्रान्त करती है। यह परमात्मा से मिला कर जीवन को पुनः उद्देश्यपूर्ण तथा गहन, महत्त्वपूर्ण और अद्भुत उपहार स्वरूप में रूपान्तरित करती है। जीवन के परिवर्तित दृष्टिकोण तथा रूपान्तरण की जीवन में ही अनुभूति का साधन, प्रमुख रूप में ध्यान है। मृत्यु की समस्या सुलझ जाती है, क्योंकि ध्यान आपको अपनी यथार्थ प्रकृति की चेतना प्रदान करता है जो आपके अमर्त्य एवं शाश्वत आत्मा का साक्षात्कार है। एवंविध यह आपको सब प्रकार के मृत्यु-भय से परे ले जा कर भय-मुक्त करता है।
ध्यान की आवश्यकता
ध्यान के उच्चतम अनुभव में आप मृत्यु का उपहास कर, इसे तुच्छ समझ सकते हैं। आपको सदा अपने अविकारी अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। आप जन्म रहित, अमर्त्य, अविकारी, अनादि और अनन्त हैं। उस अपरोक्ष ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति आपको यहीं और अभी प्रदान की जा सकती है-जन्मान्तर में अथवा उससे अतीत नहीं। इस प्रकार काया के रहते भी आप मृत्यु के भय और विभीषिका से मुक्त हो सकते हैं। आपको विदित है कि नश्वर पदार्थ पार्थिव हैं, भौतिक हैं और यह आप पर प्रभाव नहीं छोड़ता। आप शरीर में अन्तर्वास करने वाले अमर्त्य तत्त्व हैं जो शरीर के विनाश पर भी सर्वशः सदा अस्पष्ट रहता है। आपको ज्ञान है कि आप ज्योतिर्मय हैं और शरीर तथा मन से स्वतन्त्र हैं। आप अनुभव करते हैं कि शरीर की आवश्यकता नहीं है, आप इसके भीतर हों अथवा काया रहित; कोई अन्तर नहीं, यह वही है। ध्यान द्वारा इस पर विजयश्री की प्राप्ति होती है।
अनादिकाल से श्रुति ने बलपूर्वक, अनिश्चयेन बिना किसी भूल के यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य की कोई भी उपलब्धि-व्यक्तिगत अथवा जगत्-सम्बन्धी, लौकिक अथवा परलौकिक-ध्यान के द्वारा ही उपलब्ध हुई है। भारत के उत्कृष्ट वेद-ग्रन्थों ने मधुर एवं आधिकारिक वाक्यों में घोषणा की है कि ध्यान द्वारा सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की, ध्यान द्वारा ही वह महत् शक्ति भूलोक का पोषण कर रही है। अपेक्षित है कि युगों पर्यन्त ध्यानस्थ रहने के उपरान्त सृष्टिकर्ता की सत्ता से ही मात्र उसकी इच्छा शक्ति करने पर सृष्टि का उद्भव हुआ जो ध्यान द्वारा उत्सर्जित शक्ति द्वारा अजेय थी।
मानव में ध्यान-प्रक्रिया अद्भुत रूपेण कार्य करती है। मन का, इसकी चंचल और विक्षिप्तावस्था से नितान्त सूचिकाग्रवत् संहरण करके, (जिस अवस्था में यह सम्पूर्ण विश्व में भ्रमण करता है) इसकी बहिर्मुखी तथा मध्योत्सारी अर्थात् केन्द्र से हट जाने वाली वृत्तियों को वशीभूत करके, इसकी किरणों का संहरण करके, उन्हें एक बिन्दु पर केन्द्रित करके, मन को अणुवत् बना कर मनुष्य अपनी अन्तरात्मा से अनन्त शक्ति उत्पन्न करने में समर्थ है जो उसके अन्तस्तल में अन्तर्हित शक्ति के रूप में विद्यमान होती है।
मेधा और अन्तर्ज्ञान
अपने भौतिक स्वरूप की सीमाओं के कारण बाह्यतः आप ससीम हैं। आपकी शक्तियाँ भी सीमित हैं। आपकी बुद्धि सर्व विचार-प्रक्रिया को नाम और रूप पर आधारित करने की अनिवार्यता से बन्धनयुक्त है; क्योंकि नाम और रूप के बिना मन किसी विचार को ग्रहण नहीं कर सकता। अतएव नाम और रूप के देहबन्ध में ही बुद्धि की प्रक्रिया सम्भव है।
कोई भी विचार अपने आधार के लिए नाम, आकार अथवा स्वरूप का आश्रय ग्रहण करता है। अन्तस्तम में देह और मन से परे, आपकी असीम आत्मा विराजमान है। यह वही परम चैतन्य है जो स्वाभिव्यक्ति हेतु संघर्ष करता है; परन्तु अक्षम है। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति के माध्यम सीमित हैं। आपकी आत्मा का सत्त्व अन्तस्तम असीम सारतत्त्व इन सीमित साधनों में अधिष्ठित होने के कारण इनके द्वारा स्वकीय प्रभावपूर्ण स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के प्रयास में रोका जाता है। ध्यान आपकी जीवात्मा को इस बन्धन से मुक्त करता है।
ध्यान द्वारा आप क्रिया-शक्ति प्राप्त करते हैंन्जो बुद्धि के बन्धन तोड़ती है और आप बुद्धि का अतिक्रमण कर इससे परे जा पहुँचते हैं। ध्यान आपको प्रत्येक मनुष्यात्मा में अन्तःकरण में स्थित उसे अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति अन्तर्ज्ञान की शक्ति की ओर अग्रसर करता है जिसे ज्ञानचक्षु अथवा चमत्कारिक, तृतीय नेत्र भी कहा जाता है। केवल वही शक्ति आत्मा का यथार्थ एवं न्याययुक्त साधन है। भ्रान्तिवश आप मन और बुद्धि का प्रयोग करते हैं जो अधिक-से-अधिक आपके अन्तःकरण में स्थित 'मैं', 'अहं' के साधन हैं। यह 'अहं' अथवा अहंकार, यह अल्प व्यक्तित्व, यह नाम, यह स्वरूप, यह व्यक्ति, राष्ट्रीयता, जाति, वर्ण, धर्म, ऊँचाई, रंग के असंख्य सीमित तत्त्वों से सीमाबद्ध यह भ्रान्त 'अहं' क्षणभंगुर और मिथ्या है। हमारे भीतर 'अहं' हमारा आत्मा है जो भ्रान्ति के आवरण से परे तेज से प्रकाशित है।
शुद्ध चेतन, इस आवरण-शक्ति, भ्रान्तिजनक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति से सम्बद्ध और उस सम्बन्ध से पथ-भ्रष्ट हो नाम और रूप में अभ्यास करता है और निजात्मा को एक असत्य वस्तु के रूप में ग्रहण करता है। शरीर और बुद्धि इस मिथ्या एकरूपता के अभिव्यक्ति-स्रोत बन गये हैं। इस तुच्छ 'मैं' की अभिव्यक्ति के लिए साधन-रूप में ये पर्याप्त हो सकते हैं; किन्तु 'आप' के लिए वे अत्यन्त अपर्याप्त हैं। आपको सत्ता प्रदान करने वाले सर्वशक्तिमान् प्रभु ने आपको आत्म-तत्त्व की अभिव्यक्ति हेतु साधन प्रदान किया है-साधन जो सर्वोत्कृष्ट है और वह अन्तः साधन है- अन्तर्ज्ञान।
अन्तर्ज्ञान की जागृति एवं विकास तथा विशाल असीम शक्ति का उन्मीलन ही ध्यान का उद्देश्य है और ध्यान की चरमावस्था की उपलब्धि यही है।
जीवन का उद्देश्य-ध्यान
तो क्या ये धारणा कर ली जाये कि जब तक पूर्णत्व की आत्यन्तिक अवस्था प्राप्त नहीं होती जहाँ अन्तर्ज्ञान प्राप्त होता है-शुद्ध चेतना का केन्द्र-तब तक हमारे सर्व प्रयास निरर्थक हैं, फलस्वरूप कोई प्रतिदान अथवा वरदान नहीं? इसका उत्तर सुनिश्चित नहीं है। होता इसके सर्वथा विपरीत है। ध्यान तो आपको उसी दिवस पुरस्कृत करता है जिस दिन आप उसका श्रीगणेश करते हैं। तत्काल ही आप ध्यान के आनन्द का अनुभव करने लगते हैं और परिणामस्वरूप आप प्रशान्ति, स्थैर्य, मन की स्पष्टता, सामंजस्य और शान्ति के रूप में महान् प्रतिदान प्राप्त करते हैं। ये सभी परिणाम सम्यक् ध्यान के प्रारम्भ करने के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। यही इस प्रक्रिया की महानता है।
महान् आत्माएँ, विशेषकर रहस्यवादी और सन्तगण ध्यान के प्रति इतने उत्सुक और इतने एक-पक्षीय रहे हैं कि उनमें से कतिपय ने यह घोषणा कर दी कि मनुष्य की रचना ध्यान करने के लिए हुई है। ध्यान-प्रक्रिया बुद्धि की एकमात्र और उचित प्रक्रिया मानी जाती है। जीवन के अन्य सभी पक्षों का महत्त्व तभी है जब वे आपको ध्यान-प्रक्रिया में प्रवृत्त करने को प्रेरित करें। ये महात्मा जीवन को अश्रुधारा अथवा कंटक एवं कंटक-गुल्म से परिपूर्ण वन की भाँति नहीं समझते, प्रत्युत परम आनन्द की ओर अग्रसर करने वाला सुपथ मानते हैं। वे मानव-जीवन को प्रभुप्रदत्त महान् वरदान (उपहार) समझते हैं और कहते हैं कि पारलौकिक एवं वर्णनातीत अबोधगम्य, बोधातीत असीम आनन्द और शान्ति की अनुभूति हेतु यह जीवन मिला है। अतः इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वे मनुष्य को केवल ध्यान का ही आदेश देते हैं जिससे वह अपने जीवन में पूर्णत्व प्राप्त कर सके और प्रभुप्रदत्त महान् उपहार की उपलब्धि को सफल बनाने में समर्थ हो सके।
आत्यन्तिक भगवद्-साक्षात्कार कराने की शक्ति केवल ध्यान में ही है, सृष्टि के आदिकाल से अन्य किसी प्रक्रिया का अन्वेषण नहीं हुआ। उच्चकोटि के रहस्यवादी अविला के सेन्ट टैरसा ने इसे स्वर्ग का मार्ग बताया। स्वर्ग से उनका अभिप्राय ब्रह्म की अनुभूति से था। मेघों से परे सृजित किसी बाह्य स्थान से नहीं। क्रास के सेन्ट जौन ने कहा है कि ध्यान आनन्द और अमरत्व की कुंचिका है। ईश्वर के अनन्य भक्त और प्रेमी सेल्स के सेन्ट फ्रांसिस ने कहा- "जिन प्रक्रियाओं से उसने भगवद्-प्रेम का विकास किया है, उनमें से एक अन्तरंग ध्यान है।" उन्होंने इसे आनन्द-धाम का प्रवेश-द्वार कहा। सम्पूर्ण योग की प्रमुख प्रक्रिया और केन्द्र ध्यान ही है। एवंविध, इस प्रक्रिया का वर्णन सभी ने, पूर्वीय और पाश्चात्य रहस्यवादियों ने किया है और अब भी सुदूर पूर्व (चीन और जापान) में लाओत्से-दर्शन के अनुवर्तक ध्यान की शपथ लेते हैं। मनुष्य को इसे सीमित अनित्य सत्ता से परे ले जा कर उसे अनन्त बनाने वाली प्रक्रिया को ही वे सुनिश्चित मानते हैं। इसका उद्भव भारत में हुआ। भारत में इसे ध्यान की उपाधि दी गयी और वह नाम सुदूर पूर्व भारत से बाह्य स्थानों में जाने पर कलुषित हो गया। अब अमेरिका के पश्चिमी तट में यह ज़ेन ध्यान के नाम से अत्यन्त प्रचलित हो गया है जो वस्तुतः व्यर्थ अभिव्यक्ति है। दुःखद तथ्य तो यह है कि आधुनिक अमेरिकन जेन अनुगामियों के अधिकांश लोगों ने ध्यान-प्रक्रिया के महत्त्व को पूर्णतया खो दिया।
सुख और शान्ति, अन्तरंग शक्ति वास्तविक रूप से अखण्ड, ज्योतिर्मय और आकर्षक व्यक्तित्व की आकांक्षा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ध्यान परम महत्त्व का विषय है। जीवन के प्रत्येक स्तर पर ध्यान आप पर आध्यात्मिक प्रकृति और आध्यात्मिक अनुभवों के रूप में पारितोषक की वृष्टि करता है।
ध्यान-प्रक्रिया
इस विज्ञान में पारंगत आचार्यों द्वारा प्रदत्त नियमों के आधार पर अब हम ध्यान की परिभाषा पर विचार करेंगे। मूलतः ध्यान मन की प्रक्रिया में मन के साथ बुद्धि का भी योग है और इसीलिए यह अपने वास्तविक स्वरूप में सर्वशः आभ्यन्तर है और आपकी अन्तरात्मा की स्थिरता में ही इसका अभ्यास सम्भव है। मनोयोग के महत्त्व विज्ञान के रचयिता, पूर्व के महान् सन्त पतंजलि ने ध्यान के विषय पर विश्व के समक्ष एक अत्यन्त पूर्ण एवं वैज्ञानिक कार्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने ध्यान की परिभाषा 'अनवरत अखण्ड एकाग्रता' अथवा 'एक ही विषय पर एकाग्र मन का सतत प्रवाह' शब्दों में की है। इसका अभिप्राय है कि ध्यान का एक विशेष लक्ष्य होता है जिसके ऊपर मानो एकाग्र मन को आरूढ़ किया जाता है। एकाग्र मन को इस अवस्था में प्रक्षिप्त किया जाता है और विचारधारा के प्रवाह अथवा गतिशीलता को अटूट रखा जाता है। इसकी उपमा एक पात्र से द्वितीय पात्र में तेल के प्रवाह से की जा सकती है। यही ध्यान है।
ध्यान की प्रक्रिया अनिवार्यरूपेण अनन्यमनस्कता को उपलक्षित करती है। एकाग्रता स्वतः अर्थव्यंजक है, द्योतक है। इसका तात्पर्य है मन को एकाग्रचित्त करना और अन्तर्निहित संहृत और एकीकृत लक्ष्य की ओर केन्द्रित करना। इस अनुशासन की पूर्वावस्था में मन को किसी बाह्य लक्ष्य पर भी केन्द्रित किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया मनोप्रशिक्षण की कला है।
ध्यान-प्रक्रिया के इस नितान्त बाह्य पक्ष से आपको विदित होगा कि मन पूर्वतः ही बहिर्मुखी है और आप मन को किसी विषय-सुख, किसी अनुभव, व्यक्ति अथवा किसी स्मृति पर एकाग्र करके केन्द्रित करके प्रशिक्षित करते हैं। जिससे बहिर्मुख मन, जो पूर्वतः ही सैकड़ों विषयों में विकीर्ण है, अन्तर्मुख हो जाता है। तदनन्तर इस महती ध्यान की प्रक्रिया में प्रमुख साधन सम्मुख आते हैं-
(क) बाह्य विश्व में असंख्य विभ्रान्त विषयों से मन की विकीर्ण रश्मियों (वृत्तियों) का संहरण;
(ख) एवंविध संहत मन को एक लक्ष्य पर एकाग्र करना; और
(ग) सतत एकाग्रता में निमग्न मन का निग्रह, जिसमें किसी बाह्य विचार को प्रवेश की आज्ञा न हो।
अतः आपके द्वारा संयमित विचार के विपरीत अन्य सभी वृत्तियों को बाहर ही निग्रहीत रखना ध्यान है। शनैः शनैः क्रमशः यह अधिकाधिक उग्र किया जाता है और आपका ध्यान गहन से गहनतर होने लगता है।
यह सरल प्रक्रिया है-विक्षिप्त मन को संहृत करो, इसे एक केन्द्र अथवा विचार पर एकाग्र करो, इसे सतत एकाग्रित रखो और साथ ही सभी विपरीत विचारों का निराकरण करो, निमज्जन करो और विगाहक की भाँति गोता लगाओ जो अमूल्य मौक्तिक (मोती) प्राप्त करने के लिए उदधि की गहराई में जाता है। मौक्तिक ऊपरी सतह पर नहीं तैरते।
ध्यान का द्वार-चरित्र
यह प्रक्रिया भी अति-सरल है; यह उस प्रक्रिया हेतु पूर्वोद्यतन है जो जटिल है। यदि आप व्हाइट हाऊस में राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, तो यह अत्यन्त सरल है। इसमें कुछ भी विशेष नहीं। यद्यपि आत्यन्तिक प्रक्रिया पर्याप्त सरल है, तथापि अनेक औपचारिकताएँ और अन्य विघ्न जो आपके समक्ष आने हैं और जिन्हें आपने अतिक्रमण करना है जिससे कि आप उसके समक्ष खड़े होने की अवस्था प्राप्त कर सकें और आपको केवल हाथ उठाना है और उसके हाथ से मिलाना है। यह सब तैयारी अनेक मास पर्यन्त हो सकती है। आपको राष्ट्रपति के कार्यालय से समस्त विश्वास-पत्र लेने होंगे और दर्शन की तिथि निश्चित करनी होगी। तदन्तर आपको विमान अथवा रेलगाड़ी की सीट रिजर्व करानी होगी, वाशिंगटन में वास-स्थान निश्चित करना होगा।
इसके पश्चात् वास्तव में 'व्हाइट हाऊस' में प्रवेश करने पर आपको ज्ञात होगा कि आपसे पूर्व अनेक लोग आये हैं और राष्ट्रपति के दर्शनार्थ आपको दीर्घ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इसी प्रकार से यदि आप गहन ध्यान की प्रक्रिया द्वारा पावन से पावनतम में प्रविष्ट होने की जिज्ञासा रखते हैं, तो इसके लिए तैयारी करने में आपका पर्याप्त समय, शक्ति और प्रयास व्यय हो सकता है। ध्यान के विषय पर आपको दर्जनों आचार्यों की खोज करके उनसे बात करनी पड़ सकती है। अभ्यासरत अन्य आचार्यों के साथ विविध प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करो। पुस्तकों एवं उपदेशों द्वारा अपने अन्वेषण में प्रवृत्त रहो। ध्यान की प्रक्रिया तो सरल है; किन्तु इसकी ओर मन को प्रवृत्त करने की तैयारी दीर्घकालीन एवं जटिल है।
सर्वप्रथम, मन (चित्त) स्थूल अवस्था में होता है। स्थूल चित्त वृत्तियों को शान्त नहीं कर सकता। केवल सूक्ष्म चित्त ही एकाग्र हो सकता है। शुद्ध चित्त ही सूक्ष्म होता है। अशुद्ध चित्त स्थूल होता है। मन का वह भाग जो यौगिक भाषा में 'चित्त' कहलाता है, वह मनुष्य की प्रकृति के पूर्णतया शुद्ध न होने पर स्थूल रहता है। इसका आशय क्या है? क्या इसका अभिप्राय यह है कि साबुन और जल के साथ प्रक्षालन की आवश्यकता है। नहीं! इसका अभिप्राय यह है कि मानव-प्रकृति दोषपूर्ण है और इन दोषों का निराकरण करना है।
यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। ध्यानस्थ होने के लिए कतिपय विशेष परिस्थितियों का निराकरण अनिवार्य है। ये दोष मानव-प्रकृति की अशुद्धताएँ-निष्ठुरता, उत्तेजना, अल्प तुच्छ ईर्ष्या से लोभ, मोह, घृणा, काम, क्रोध, अहंकार, दर्प, भ्रम और स्पृहा पर्यन्त कुछ भी हो सकता है। ये सब दोष प्रकृति को अत्यन्त स्थूल, अशिष्ट और अधम बनाते हैं। वे पूर्ण रूप से अनात्मिक हैं और मन को अस्थिर बनाते हैं तथा दोलायमान करते हैं। अतएव उनका पूर्ण रूप से निराकरण करना है और यही मूल कार्य है, सिद्धि-साधन है जो इतना सहज नहीं है। यह अनुशासन यद्यपि स्पष्ट रूप से नैतिक है, तथापि योग की वैज्ञानिक कला पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यह मूल आधार ही विरचना करता है जिस पर योग के स्वरूप का विकास किया जाता है।
योग का गौरवशाली विज्ञान जो आपको ध्यान की ओर अग्रसर करता है, नैतिक जीवन और सम्पूर्ण धार्मिक न्याय पर आधारित है। नितान्त भद्र, पूर्ण चरित्र युक्त उपमा, सदाचार के पथ एवं सर्वोच्च गुणों से युक्त जीवन की ओर सतत निर्देश करती है सब महान् उपलब्धियों, अयुक्त प्राप्तियों, जो सूक्ष्म वायु में नष्ट नहीं होतीं, जो न केवल इस भौतिक तल पर ही सीमित हैं, प्रत्युत चिरस्थायी और शाश्वत हैं, इनके स्थिरीकरण का एकमात्र साधन गुण धर्म है। सर्व दोषों का पूर्ण निराकरण, सर्व उच्चतर उपलब्धियों का मूल और आधार है। ध्यान में सफल होने के लिए मन की शुद्धि अनिवार्य है और यदि मन शुद्ध है, तो आपको सात्त्विकता में विकसित होना है, गुणों का विकास करना है, अपने स्वभाव से घृणा और कठोर का सम्पूर्णतया निराकरण करना है।
दूसरों के प्रति दया भाव रखो। मन, वचन और कर्म से दयालु बनो। आपकी वाणी मधुर हो, आपके कर्म सहानुभूतिपूर्ण हों। वस्तुतः आपको स्वभाव से देवतुल्य बनना चाहिए। यह अनिवार्य है; क्योंकि दैवी गुणों से सम्पन्न आत्मा ही दिव्य स्वरूप हो सकती है। आपको ईश-प्रकृति प्रतिबिम्बत करनी है। ईश्वर यदि आपका अवलोकन करें, तो स्व दिव्य प्रकृति के प्रतिबिम्ब का आपमें अनुभव करें। वह प्रकृति अंकुरित हो, अनावृत हो तथा दिव्य पुरुष की भाँति मानव-प्रकृति रूपी क्षेत्र में विकसित हो। सात्त्विक जीवन में यह संवर्धन ही दुष्कर है; क्योंकि मानव-प्रकृति में स्वाभाविक लक्षण सहज ही विनष्ट नहीं होते। पुनरपि आप तत्परता से उनके निराकरण का प्रयास करें; पुनः-पुनः आप किसी-न-किसी रूप में उन्हें अंकुरित होता देखेंगे। काम, लोभ और तृष्णा को प्रकृति से सहजरूपेण जड़ से उखाड़ना है। ध्यान के महान् आचार्य पतंजलि ने कहा है कि दिव्य प्रकृति में रूपान्तरित होने का सर्वाधिक प्रभावपूर्ण साधन अल्प दुर्बलताओं को वानर की भाँति जूँ निकालने के समान नहीं, जो समय और शक्ति का हास है, प्रत्युत स्वयं को गुणी बनना है।
अतएव व्यक्त रूप से हठात् भद्रता का विग्रह बनो। अधिकाधिक सत्यनिष्ठ बनो, करुणार्द्र बनो, प्रत्येक चरण पर सहायी भाव निःस्वार्थपरता एवं सेवाभाव अभिव्यक्त करने का अवसर खोजो। एवंविध साक्षात् रूप से वपन एवं सक्रिय अभ्यास से आप सात्त्विकता का विकास करते हैं। यदि आप भद्रता के लिए व्यग्र आसक्ति का विकास करें, तो निषेधात्मक पक्ष का लोप हो जायेगा। आप यदि प्रकाश को आभासित करें, तो अन्धकार इसके समक्ष नहीं रह सकता। इसी प्रकार ही निजात्मा को पूर्णत्व से परिपूर्ण करने पर आप सर्व दोषों का प्रक्षेपण कर देंगे और एक आदर्श जीव के रूप में संवर्धित होंगे।
इसका ध्यान के साथ सीधा सम्बन्ध है। ध्यान की महती विधियों में एक स्वयं को पवित्र और पूर्ण सत्ता में विकसित करना है। दो प्रक्रियाएँ परस्पर अन्तः सक्रिय हैं। ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में अवतीर्णार्थ आपको पूर्ण अखण्ड बनना होगा और अखण्डता की प्राप्ति के लिए आत्म-शक्ति को प्रोत्साहित करके, विचार शुद्धि, मेधा की प्रवीणता एवं इस प्रकार से विवेक-शक्ति के विकास द्वारा ध्यान इन दोषों एवं दुर्बलताओं का अतिक्रमण करने के लिए सर्वाधिक सहायी है। आप युक्त-अयुक्त का निश्चय करने में अधिक समर्थ हो जाते हैं और आत्म-विश्लेषण हेतु आप और अधिक समाहत हो जाते हैं; क्योंकि मन एकाग्रता और ध्यान द्वारा अभेद्य हो जाता है। यह सूक्ष्म और कुशाग्र हो जाता है।
एकाग्र मन की शक्ति
एकाग्रित मन ही निपुणता और शक्ति से कार्यरत रह सकता है। एकाग्रचित्त शक्ति से प्रत्येक क्षेत्र में सभी विशिष्ट उपलब्धियों पर विजय प्राप्त की गयी है। राजनीति- विशारद, युद्ध-कौशल, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अन्वेषक और शल्यचिकित्सकों ने एकाग्रचित्त शक्ति से ही सफलता प्राप्त की है।
उनका चित्त 'एक-पथ-गामी' था। उन्होंने स्वयं को ऐसा ढाल लिया था। उन्होंने विचारपूर्वक एक-पथ-गामी भावना का विकास किया। आइन्सटिन यदि ध्यानपरक नहीं, तो और क्या था? ध्यान में वह विराट् ब्रह्माण्ड के अन्तस्तम रहस्यों का सूक्ष्म-परीक्षण करने में सक्षम था और उसी में सत्य उसके समकक्ष आविर्भूत हुए। उसे सत्य का प्रकाश हुआ। उसका अन्तर्ज्ञान प्रदीप्त हुआ और उसे लौकिक रहस्यों के अन्वेषणार्थ प्रेरणा प्राप्त हुई जिनके द्वारा पश्चात्काल में उसने विस्मयकारी समीकरण की सूत्ररूपेण रचना की।
इन महान् पुरुषों के सभी एकाग्र भाव बाह्य थे। उन्होंने स्वचेतना में जिस प्रक्रिया को अपनाया, वह आभ्यन्तर नहीं थी। नश्वर नाम और रूपों के अचिरस्थायी जगत् की दृष्टिगोचर सत्ता के बाह्य विश्व पर उन्होंने चित्त को केन्द्रित किया। महानतम ज्योतिःशास्त्रज्ञ एवं वैद्यों ने बाह्य पदार्थों पर गहन चिन्तन किया और उनका ध्यान अन्तःस्थित 'सत्य' पर केन्द्रित होने की अपेक्षा बाह्य विश्व पर अधिष्ठित हुआ।
अतएव गतिशील जगत् की अद्भुत उपलब्धियाँ प्राप्त कर लेने पर भी वे आत्यन्तिक एवं शाश्वत सत्य परमात्मा को न पा सके। उनके प्रयास सर्वविध अनवरत श्लाघ्य एवं प्रशस्य थे। वे सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ हैं जो कभी अपने चित्त को एकाग्र नहीं करता, जिसे यह ज्ञान नहीं कि मनोनिग्रह क्या है और एकान्त चिन्तन क्या है, जिसे यह भी ज्ञात नहीं कि ध्यान में उन महान् सत्यों का उन्मीलन करने की शक्ति है जो दृष्टिगोचर ब्रह्माण्ड की सतह में अन्तर्निहित हैं। इस धरती पर अधिकांश लोगों को इस शक्ति का ज्ञान नहीं है। यह वह वस्तु है जिससे वे संकेत मात्र भी परिचित नहीं।
विचार (प्रक्रिया) के नियम
विचार-नियों के अनुष्ठान द्वारा जीवन के महान् सत्यों की अभिव्यक्ति में ध्यान अद्भुत रूप से सफल हुआ है। विचार का प्रथम नियम है-कोई भी विचार जो मन में चिरकाल से साहसपूर्वक दृढ़ता से वास करे, वह तथ्य रूप में संहत हो जाता है।
यह अविविक्त तथ्य की भाँति यथार्थ बन जाता है। यह महान् नियमों में से एक है जिस पर विचार-शक्ति का ज्ञान आश्रित है। अन्य नियम आध्यात्मिक हैं जो मानसिक और बौद्धिक स्तर तक सीमित नहीं हैं, प्रत्युत गहनतर एवं इससे अतीत हैं और उच्चतर हैं। यह नियम इतना गम्भीर एकाग्रित विचार है जो अपने आत्यन्तिक अन्त तक साग्रह अवस्थित है और अकस्मात् ही बुद्धि और मन से परे छलाँग मार कर अन्तर्शन के धाम में प्रवेश करता है। यही विधि का विधान है। जब मन पूर्णतया एकाग्रित एवं ध्यान-प्रक्रिया में अत्यन्त लीन होता है, यह अन्तर्धान हो जाता है और आप शुद्ध चेतन के अनुभव में निविष्ट होते हैं। यह विद्युत् प्रवाह की भाँति है जो स्विच दबाने पर वृत्तखण्डीय प्रदीप (लैम्प) में पहुँचता है। वृत्तखण्ड के एक कोने तक वेग से पहुँचने पर यह अकस्मात् ही विद्युद्वेग से शून्य स्थान को क्षण भर में पूर्ण करता हुआ पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठता है।
इसी रोमांचक और उत्कृष्ट आन्तरिक अनुभव में आप सापेक्ष और निरपेक्ष के मध्य के शून्य स्थान को मानो छलाँग मार कर पार करते हैं, आप सवपिक्षता और दृष्टिगोचर वस्तु का अतिक्रमण करके असीम अनुभव प्राप्त करते हैं। ससीम जीव-चैतन्य के तुच्छ बन्धन से, असीम और अनन्त दिव्य चैतन्य की उत्कृष्ट विशालता में यह विजयपूर्ण छलाँग है; यह एक परा-मानसिक परमानुभूति है जिसमें ध्यान, ध्याता और ध्यान का विषय, तीनों अभिन्न एकत्व में एकरूप हो जाते हैं। तीनों अनिर्वचनीय अनुभव, अक्षय्य शान्ति और असीम आनन्द एवं जाज्वल्यमान् ज्योति में लीन हो जाते हैं।
अन्ततः ध्यान की ही यह महती प्रक्रिया है जो ईश्वर के साथ आपका सम्पर्क स्थापित करके आप पर अमरत्व की वृष्टि करती है। आपके दैनिक जीवन में ऐसा क्या है जो एकाग्रता का विकास करने में आपका सर्वाधिक सहायी हो? व्यक्ति किसी भी अनुष्ठान में रत हो, वह एकाग्रता की योग्यता का विकास कैसे करता है? आप तश्तरी धो रहे हों, अपना खाता लिख रहे हों, शिशु के लिए कुछ मिश्रण तैयार कर रहे हों, पत्र लिख रहे हों, किसी लिफाफे से टिकट उतार रहे हों, मेज की ऊपरी सतह झाड़ रहे हों-आप जिस किसी कार्य में भी रत हों, इसे सावधानी से एकाग्र रूप से करो। इसे पूर्ण अनन्यमनस्कता से करो। एक समय में अन्य विचारों का चिन्तन मत करो। यह एक कला है, जो समय-समय पर अतीव उपयोगी सिद्ध हो सकती है विशेषतया जब आपको नगर से बाहर किसी होटल में प्रतीक्षा करनी पड़े; पर ध्यान के लिए ऐसा नहीं है। यदि आप एक ही समय में दश बातों का चिन्तन करेंगे, तो आप एक निपुण सेवक अथवा हवाई अड्डे पर यात्रा रिजर्वेशन क्लर्क बन सकते हैं, किन्तु इस प्रकार का स्वाभाविक मिश्रित और विविध चिन्तन ध्यानार्थ सहायी न होगा।
अतएव चिन्तन और कर्म में विशिष्ट एवं स्थिर बनने का प्रयास करो। स्वप्रकृति को एकाग्र भाव में विकसित करो। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक शीघ्र आप मनोयोग के स्वभाव में परिणत होंगे। आपका अभ्यास दैवाधीन अथवा कभी-कभी नहीं होना चाहिए। यह नियमित होना चाहिए और आपको पूर्ण वर्ष-पर्यन्त तीव्र एकाग्रता जागृत करने के लिए कुछ अभ्यास करना चाहिए। ऐसे अभ्यास में संलग्न होने पर आप अनुभव करेंगे कि आप अद्भुत रूप से एकाग्रता-शक्ति का विकास कर रहे हैं और जहाँ भी आप अपना चित्त एकाग्र करते हैं, यह वहीं स्थिर रहता है। सततरूपेण किसी आभ्यन्तर वस्तु पर चित्त एकाग्रित करना ध्यान का विषय है। ध्यान में सफलता एकाग्रता पर निर्भर है। एकाग्रता अभ्यास से आती है और अभ्यास स्वभाव से नियमित हो जाता है। यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करें, तो आप ध्यान में सफल होंगे और ऐसा अभ्यास तभी सम्भव है, जब आप यथार्थ रूप से और गम्भीर रूप से सम्पूर्ण प्रक्रिया में रुचिबद्ध हों।
ध्यान में शरीर, मन और प्राण की भूमिका
शरीर, मन और प्राण-सभी अन्तः सम्बद्ध हैं। अतएव शरीर को बिना हिलाये एक ही मुद्रा में स्थिरतापूर्वक आसनस्थ होने तथा प्रशान्ति में उस मुद्रा को बनाये रखने में आपको एक अन्य गरीयसी सहायता प्राप्त होती है। नित्य योगानुशासन की मौलिक अवस्थाओं में आप पायेंगे कि आपके यौगिक जीवन का आधार एक नितान्त, पवित्र, नैतिक और सदाचारी (धार्मिक) जीवन है। तब आप प्रतिदिन स्थिरतापूर्वक आसनस्थ होना प्रारम्भ कर देते हैं। एक समय-विशेष पर प्रतिदिन आपको एक प्रशान्त एकान्त स्थान में अभ्यास हेतु स्थिर मुद्रा में आसीन होना चाहिए। आप किसी कुरसी पर भी आसीन हो सकते हैं, यदि आपको यही मुद्रा हृदयग्राही लगे। इस मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, शरीर को पूर्णतया ढीला छोड़ दें, हस्त की उँगलियों को परस्पर बाँध कर घुटनों पर टिका लें और उसी मुद्रा में बैठने का प्रयास करें।
इस प्रकार जब शरीर निष्क्रिय-सा हो जाये, तो प्रथमतः मन शत-शत पृथक् दिशाओं में भागने का प्रयास करेगा। अत्यन्त अनियन्त्रित रूप से यह भागेगा; किन्तु विचलित न हों, इसे भागने दें। इससे दूर खड़े रहें; अन्तःकरण से जागृत रहें और इसकी अयोग्यता का अवलोकन करें।
कालोपरान्त आप देखेंगे कि इस उछल-कूद में एक तत्त्व खो रहा है और वह है 'आप' । आप द्रष्टा बन गये हैं। मन इस प्रक्रिया को अत्यन्त उग्र रूप में निरन्तर करता रहेगा; किन्तु अब आप उसमें रुचि नहीं लेंगे, तो यह सदा समीपस्थ चक्रों में विचरण करेगा और अन्ततोगत्वा उदधि में तैरते हुए जहाज के दण्ड के शिखर पर बैठे पक्षी की उड़ान की भाँति यह अपने अध्यास (वास यष्टि) पर पुनरावर्तन करता है। अब यह विश्श्राम लेता है। मन अब भागता नहीं और अहं-चैतन्य की सक्रिय सहायता के बिना विविध चिन्तन में प्रवृत्त नहीं हो सकता।
अतएव विचार-चक्र के साथ एकत्व स्थापित मत करो। यदि आप पृथक् और आत्म-केन्द्रित रहेंगे और अनासक्त रहेंगे, तो मन का स्वाभाविक संक्षोभ शनैः-शनैः समाप्त हो जाता है। कुछ सप्ताहों पर्यन्त अथवा इससे भी अधिक मौन-वास में रहने से आप अनायास ही अनुभव करने लगते हैं कि मन पूर्व-स्थिति से अब अधिक प्रशान्त है। अब यह इतस्ततः भटकता नहीं। यह परम आनन्द है। आप उस प्रशान्ति का लाभ उठाने का प्रयास प्रारम्भ करने लगेंगे और किसी हृदयग्राही विचार को मन में एकाग्रता हेतु आवाहन करते हैं। ये कदाचित् एक सुन्दर पुष्प का मानसिक चित्र अथवा विस्मित करने वाला स्वर जो आपने श्रवण किया हो अथवा प्रभातकाल में पक्षियों की चहचहाहट अथवा सूर्योदय, गरिमामय सूर्यास्त अथवा रंजित इन्द्रधनुष हो सकते हैं। मन को आकृष्ट एवं नियन्त्रित रखने के लिए यह कोई प्रिय वस्तु होनी चाहिए। अब मन इस पर स्थिर करें-यही प्रारम्भिक प्रशिक्षण है।
ध्यान के सतत अभ्यास से आप अनुभव करेंगे कि स्थिर मुद्रा और क्रमिक शान्ति आपके श्वास को अत्यन्त ही सूक्ष्म कर देते हैं। आपकी श्वास-प्रक्रिया भी अत्यन्त तालबद्ध हो जाती है। शरीर की निश्चलता और श्वास की सूक्ष्मता से तत्काल ही एक सर्वथा नवीन प्रसन्नता (मनःप्रसाद) का अनुभव करने लगते हैं। प्रथम बार आपको ज्ञात होगा कि नितान्त प्रशान्ति, किसी भी प्रकार की चिन्ता और विचार अथवा किसी प्रकार के निषेधात्मक चिन्तन से विमुक्त होना ही यह प्रक्रिया है। संक्षेप में, बिना किसी उपशमन-यन्त्र के मन सच्ची शान्ति, वास्तविक प्रसाद और प्रशान्त अवस्था में लीन हो जाता है।
यह आदेश आपको चित्त-प्रसादत्व का रहस्य प्रदान करते हैं। प्रथमतः शरीर स्थिर होना अनिवार्य है, श्वास सूक्ष्म तथा नियमित होनी चाहिए; क्योंकि शरीर, श्वास और मन अन्तर्निबद्ध हैं। वे मानो त्रिकोण के तीन पक्ष हैं और एक व्यक्तित्व (बिन्दु) में केन्द्रित हैं। एवंविध मन के सर्वथा प्रशान्त होने पर देखेंगे कि श्वास भी सूक्ष्म (शान्त) है और शरीर स्थिर है। यदा-कदा आपका ध्यान बाधित होता है और आप किसी वस्तु-विचार में निमग्न हो जाते हैं और अनुभव करें कि आपकी एकाग्रता जो आप किसी वस्तु-विशेष में लगाते हैं, आपकी समस्त शारीरिक एवं श्वास-प्रक्रिया को मन्द कर देती है। इसी प्रकार से जब भी आपका श्वास नियमित हो, आप अनुभव करेंगे कि आभ्यन्तर ऐक्य और साम्य आपके चित्त को अभिभूत कर देते हैं।
मनःप्रसाद हेतु श्वास-प्रक्रिया
योग के साधकों को शरीर, श्वास, प्राण और मन का समन्वय समझाने के लिए मैंने इसका विस्तार से विवरण दिया है। यौगिक श्वास-प्रश्वास प्रक्रियाओं के ज्ञान में इससे उन्हें गहनतर सूझ-बूझ प्राप्त होती है। अब इन प्रक्रियाओं में श्वास पर एकाग्रित होना है। आप लोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यह सरल क्रियाओं में से एक है जिसका अभिप्राय है-आप एक नथुने से श्वास अन्दर लें (पूरक करें) और दूसरे नथुने से श्वास बाहर फेंकें (रेचक करें)। अब दूसरे नथुने से पूरक और प्रथम से रेचक करें। इस प्रकार यह प्रक्रिया एक बार पूर्ण होती है। अब इस लोम-विलोम श्वास-प्रश्वास हेतु आप दक्षिण हस्त के अँगूठे से दक्षिण नथुने को बन्द करें और वाम नथुने से श्वास खींचें। पूरक पूर्ण होने पर आप वाम नथुने को अनामिका और मध्यमा अँगुलियों से बन्द करें और साथ ही दक्षिण नथुने से अँगूठा हटा कर शनैः-शनैः उत्तरोत्तर सुखपूर्वक उसी से रेचक करें।
आप अनुभव करेंगे कि श्वास-प्रश्वास की इस प्रक्रिया से आपके चारों ओर का संसार अदृश्य हो जाता है। आपको इस शरीर का ध्यान भी नहीं रहता, प्रत्युत आप पूर्णतया प्राण पर ही एकाग्रित होते हैं। व्यतीत हो रहे समय का भी इसमें अभास नहीं रहता।
इस प्रक्रिया में संलग्न आधा घण्टा व्यतीत हो जाने पर भी कदाचित् ही आपको समय का आभास हो। कारण क्या है? क्योंकि यह नितान्त विराट् प्रक्रिया है। शारीरिक स्तर पर श्वास-प्रश्वास जीवन की प्रमुख प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समस्त जीवन को पुष्ट करती है और जब आप इसमें संलग्न होते हैं, आपका सम्पूर्ण मन गम्भीर रूप से लीन हो जाता है। अतः यह अत्यन्त अमूल्य साधनों का सार है जिसका आप प्रशान्ति एवं मनोनिग्रह की प्राप्ति हेतु अभ्यास कर सकते हैं।
इस अभ्यास से पूर्व तथा प्राणायाम की प्रारम्भिक अवस्थाओं में अभ्यास अत्यन्त सरल है। आप सुखपूर्वक एक स्थिर मुद्रा में आसीन हो जायें और शान्तिपूर्वक दोनों नथुनों से रेचक और पूरक करें। किसी प्रकार की जटिलताएँ नहीं हैं। आप यह गहन और तालबद्ध प्राणायाम-प्रक्रिया दश-बारह दिवस पर्यन्त करें। अथवा कुछ सप्ताह पर्यन्त प्रातः-सायं करें। आप अनुभव करेंगे कि आपका चित्त अधिकाधिक प्रशान्त एवं स्थिर होने लगा है। जो बातें पहले आपको व्याकुल और उत्तेजित करने वाली थीं, अब और अधिक ऐसा करने में सक्षम न होंगी। आप अनुभव करेंगे कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, मन पहले से उस पर एकाग्रित और केन्द्रित होने की प्रशान्त अवस्था में है। इसके पश्चात् आप श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया के प्रारम्भ में आप वाम नथुने से पूरक करें और दक्षिण नथुने से रेचक करें और पुनः दक्षिण नथुने से श्वास भीतर खींचें और वाम नथुने से श्वास बाहर फेंकें। छह बार ऐसा अभ्यास करें अर्थात् छह चक्र प्रातः और छह चक्र सायंकाल, जब आपका उदर अधिक न भरा हो। मध्याह्न अथवा रात्रि के भोजन के तत्काल बाद ही नहीं, प्रत्युत भोजन से एक घण्टा पूर्व ऐसा अभ्यास करें। लगभग एक मास पर्यन्त ऐसा अभ्यास कर लेने के उपरान्त शनैः शनैः कुछ क्षणों के लिए पूरक करके कुम्भक (श्वास रोकने की प्रक्रिया) का अभ्यास करें। कुम्भक की अवस्था में आपको अनुभव होगा कि मन स्थिर और शान्त है। इसका लाभ उठायें, किसी चिह्न अथवा वृत्ति पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इन अवस्थाओं में आपकी एकाग्रता विस्मय-विमुग्ध करने वाली होगी; क्योंकि श्वास रोकने पर मन अचल हो जाता है और वृत्तियाँ आपके वशीभूत हो जाती हैं।
श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया की अन्तिम अवस्था में पहुँचने पर अर्थात् कुम्भक सहित रेचक और पूरक का अभ्यास करने के पश्चात् शनैः-शनैः कुम्भक का समय बढ़ाने का अभ्यास करें। सभी जन इस प्रक्रिया को नियमित रूप से कर सकते हैं। इन प्रक्रियाओं के लिए २-३ बातों का ध्यान रखें :
(१) आपके अभ्यास में कुम्भक सदा सुखपूर्वक और सहज ही होना चाहिए।
(२) आपको ऐसा अनुभव कदापि न हो कि आपका श्वास अवरुद्ध हो रहा है अथवा कुम्भक
हठपूर्वक कर रहे हों।
(३) आप जब पूरक करने लगें, तो आपको आभास हो कि आप चाहने पर श्वास अभी कुछ समय और रोक सकते थे।
(४) पूरक सदा सहज, अत्वरित एवं अहिंसक होना चाहिए। हठ कदापि नहीं करना चाहिए। यदि यह हठपूर्वक और शीघ्र हो, तो इसका अभिप्राय है-आपने कुम्भक अपनी क्षमता से अधिक काल तक किया है और आपके फेफड़े अब और अधिक इसको निग्रह नहीं कर सकते। कुम्भक में सावधानी बरतने से आप अनुभव करेंगे कि पूरक अतीव सहज और सुन्दर रूप से हो रहा है। इसे युक्तिपूर्वक करें।
कुम्भक तभी करें, जब आप ऐसा अनुभव करें कि अब फेफड़े तो फूल (भर) गये हैं; किन्तु उन पर दबाव नहीं डालना। जब श्वास रोकते हैं, तब एक प्रकार की तालबद्ध गणना करें जिससे कुम्भक का समय नियमित हो सके। यह गणना उत्तरोत्तर बढ़ाते जायें। ऐसा व्यवस्थित रूप से करने पर आपको अनुभव होगा कि मन विस्मयात्मक अल्पकाल में ही सफलतापूर्वक स्थिरतर हो जाता है।
मन संयत हो और आपको वृत्ति-निरोध का साधन ज्ञात हो जाये तो स्थिरता मनस्तत्त्व की सामान्य अवस्था बन जाती है। वस्तुतः जिसे आप पूर्ण करने का अभ्यास करते हैं, वह उतना सक्रिय मन नहीं है जितना की वास्तविक मनस्तत्त्व है। एवंविध जब यह मन के साथ ऐसा अभ्यास किया जाता है, दृढ़ता और स्थिरता की अवस्था में रखा जाता है-मन का एक विशेष गुण जो ज्योतिर्मय है, जो सामंजस्य और समन्वय की प्रकृति का है, वह बढ़ जाता है। इसे सतोगुण कहते हैं जो अन्तःकरण का एक विशेष आध्यात्मिक गुण है। मनस्तत्त्व में इस गुण का आधिक्य होने पर सम्पूर्ण मन समन्वित, सन्तुलित और दृढ़-सा होने लगता है और वही सन्तुलन आपके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को लक्षित करता है। प्रकृति में समगुण प्रधानता होने से आप समभाव हो जाते हैं। अब आपको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। दिन-भर के श्रम के उपरान्त भी आप मन से प्रशान्त और सौम्य अनुभव करते हैं। आपको कोई अव्यवस्थित नहीं कर सकता। यह प्राणायाम, स्थिर मुद्रा, एकाग्रता और ध्यान के अभ्यास का स्वाभाविक परिणाम है।
ध्यान-लौकिक एवं आध्यात्मिक
अब इस विषय पर विचार करने से पूर्व हमें एक भेद को दृष्टि में रखना है। कहा गया है कि एकाग्रित वृत्ति की कोई भी प्रक्रिया ध्यान है। ध्यान-प्रक्रिया का अभ्यास सभी लोग करते हैं। उदाहरणतः मैंने ऐसी समीक्षा की है कि प्रायः वैज्ञानिक ध्यानी होते हैं। अन्वेषक, नीतिज्ञ और नेपोलियन जैसे महान् युद्ध-विद्या-विशारद-सभी ध्यानी थे। युद्ध-विद्या विशारद नेपोलियन ने पूर्वतः ही समर-भूमि को सूक्ष्मतम विस्तरण में रेखांकित कर लिया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसे विशाल भवन इंजीनियरों के द्वारा उत्खनित किये गये, जिन्होंने एकाग्रता और ध्यान के उपरान्त अपनी योजना को समक्ष रखा। अनिवार्य प्रत्येक कील, द्रव्यों का एक-एक औंस, प्रत्येक कोण एवं जोड़ स्पष्ट रूप से नीले अक्षरों में अंकित किये गये थे। इस स्वरूप में ध्यान-प्रक्रिया स्वयं में शुद्ध रूप से वैज्ञानिक प्रक्रिया है; परन्तु योग में इसका अनुष्ठान शुद्ध रूप से आध्यात्मिक है, भौतिक अथवा लौकिक नहीं।
इस प्रकार जब मैं आपके समक्ष ध्यान के विषय में कुछ कहता हूँ तो ध्यान से मेरा अभिप्राय अन्तर्निहित तत्त्व से होता है जो असीम आनन्द, शान्ति का वारिधि, सौन्दयाँ के सौन्दर्य और प्रकाशों का ज्योति प्रकाश है। हमें उसी से अभिप्राय है, इस विश्व से नहीं। यदि ध्यान कुशाग्र मेधा, चित्तैकाग्रता की शक्ति, महानतर व्यक्तिगत आकर्षण जीवन में महानतर सफलता, गरीयसी प्रारब्ध की आधिभौतिक उपलब्धियों की हम पर वृष्टि करता है, तो करने दो। हम इनका सुस्वागत करेंगे। उन्हें सह-उपज के रूप में आने दो। यदि वे नहीं आतीं, तो हमें उसकी चिन्ता नहीं; क्योंकि हमें तो परम, सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, महानतम तत्त्व की आकांक्षा है जिसके साक्षात्कार हेतु हमें मानव-देह प्राप्त हुई है। हमें उस सत्य सत्ता पर ध्यानस्थ होना है। हमें ब्रह्म में गोता लगा कर निज सत्ता को पूर्णतया ब्रह्म में लीन करना है। चित्त को समग्र रूप से परिपूर्ण एवं ब्रह्मलीन होने दो।
हमारे लिए ध्यान की प्रक्रिया आन्तरिक स्नान की भाँति है। यह तो एक प्रकार से श्वेत वस्त्र को वर्णयुक्त कुण्ड में भिगोने के समान है। एक बार रंग चढ़ने के पश्चात् पुनः यह विवर्ण नहीं होगा। ध्यान की भी यही दशा है। अपनी सम्पूर्ण सत्ता एवं व्यक्तित्व को दिव्यत्व के रंग में रंगना ही ध्यान है। यह अपनी समस्त मानव प्रकृति, भौतिक प्रकृति, सब वृत्तियों और भावों को भगवद्-प्रकृति में प्रवृत्त करना है। वही परम ध्यान है जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें भगवान् ने यह शरीर, बुद्धि, जीवन और यह सुअवसर प्रदान किया है। सन्तों और महात्माओं के रूप में उसने हमें महान् सेवक भी दिये हैं जो हमें स्मरण कराते हैं कि ध्यान प्रभुप्रदत्त अमोघ उपहारों में से एक है। इसकी विद्यमानता का, जब तक आपको कोई आ कर और चिल्ला कर आभास न कराये, यह आपके पास अनन्वेषित पड़ा रहता है और इसके पश्चात् आप अनुभव करते हैं- "ओहो! यह पूँजी तो मेरे पास सदा से थी; परन्तु मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया।”
परमात्मा ने ध्यान और साक्षात्कार के लिए आपको यह मनुष्य-जन्म प्रदान किया है। एक दिन भी ध्यान के बिना मत व्यतीत होने दो। कितने भी विघ्न क्यों न आयें, परिवेश कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, आप इनकी चिन्ता न करें। प्रत्यार्ह प्रातः-सायं एकान्त में अन्तर्मुख होने तथा आराधना भाव में उस परमात्मा के समीप उपासना का समय निकालें। यदि आपके हृदय में उसके लिए प्रेम है, तो आपके साधन-पथ में ऐसी कोई बाधा नहीं आ सकती जिसका आप अतिक्रमण न कर सकें। आप अनन्त काल से समय ले सकते हैं और समय का सृजन कर सकते हैं। आप २४ घण्टे के २५ घण्टे भी बना सकते हैं।
आइए, मैं आपको इसका रहस्य बताऊँ। ध्यानस्थ होने का स्वभाव विकसित करने पर आप अनुभव करेंगे कि आपके पास समय बढ़ गया है; क्योंकि जिन कार्यों को पूर्वतः आप प्रमादपूर्वक करते थे, अब उन्हीं को आप कुशलतापूर्वक शीघ्र करने में सक्षम हो गये हैं। यदि आप व्यवसायी हैं, तो जिन कार्यों को करने में दश घण्टे लगते थे, अब नौ घण्टों अथवा सात घण्टों अथवा इससे भी कम समय में सम्पन्न हो जायेगा। क्योंकि पुनरपि इस प्रक्रिया में मन-रूपी यन्त्र को परिपक्क करके इसे एकाग्रित कर रहे हैं। तत्काल वस्तुग्रहण की क्षमता भी आप प्राप्त करते हैं। अब मन विक्षिप्त नहीं रहा। ऐसा मन सभी कार्य सम्पन्न कर सकता है।
प्रारम्भावस्था में कदाचित् आपको ऐसा आभास होगा कि इस ध्यान-प्रक्रिया का स्वभाव बनाने में अल्प समय लगता है और अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त समय नहीं रहा। बिना किसी संकोच के उन कार्यों को त्याग दें। अचिरेण ही आप अनुभव करने लगेंगे कि यही ध्यान-प्रक्रिया जिसमें प्रारम्भ में आपका बहुत समय व्यतीत होता, आपको प्रतिफलस्वरूप अधिक समय और संयुक्त रुचि प्रदान कर रहा है। आपको इसका अनुभव करना है।
हम सभी ब्रह्म-जिज्ञासुओं को सदा स्मरण रखना चाहिए कि ध्यान में सफलता उस परमात्मा के प्रति हमारे प्रेम के परिणाम पर निर्भर है। जितना अधिक हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उतना ही अधिक हमारी वृत्ति उसकी ओर आकृष्ट होती है; जितना अधिक आकर्षक हम अनुभव करते हैं उतना ही अधिक ध्यान का हम आनन्द लेते हैं। अचिरेण ही चित्तवृत्ति की एकाग्रता का दुष्कर कृत्य मधुर बन जाता है और एक बार वह आनन्द-स्रोत आप खोज लें तो पुनः कदापि ध्यान के लिए किसी उद्बोधक की आवश्यकता नहीं होगी। हमें स्वयं ही शीघ्र इससे विरत होने की अनिच्छा होगी।
ध्यान में सफलता के साधन
ध्यान-पथ पर सफलता प्राप्त करने के लिए महान् रहस्यवादियों के कतिपय अमोघ आदेश इस प्रकार हैं:
(क) निरन्तर स्मरण;
(ख) सतत प्रार्थना भाव;
(ग) दिव्य नाम-जप।
यदि आप निरन्तर प्रभु-चिन्तन (स्मरण) का अभ्यास विकसित करें, तो आप अनुभव करेंगे कि मन सदा उसी विचार से परिपूर्ण रहता है। प्रगाढ़ रूप से इसी में प्रवृत्त रहो। आप जब ध्यानस्थ होने लगेंगे, तो अन्तःकरण तो पूर्वतः ही उसी भाव में निमग्न होने लगेगा। तब विशेष रूप से तत्काल ही मन उसी दिशा में प्रवाहित होने लगेगा। नित्य-स्मरण का स्वभाव बनाने के लिए सन्तों ने हमें कुछ अमूल्य आदेश दिये हैं। नित्य-स्मरण त्रिविध हो सकता है। यह आपकी बाह्य प्रकृति का अंश हो सकता है अर्थात् कुछ बाह्य तत्त्वों के द्वारा आप उस परम लक्ष्य के प्रति सजग हो सकते हैं; अथवा यह आन्तरिक कल्पना की प्रकृति का हो सकता है अथवा विवेक-शक्ति द्वारा यह बुद्धि से हो सकता है।
बाह्य तत्त्व निम्न प्रकार हो सकते हैं-दीवार पर लगे भगवान् के चित्र, पावन देव-प्रतिमा, क्रास पर ईसा का चित्र, दीपिका, कोई गोल आकृति अथवा धार्मिक ग्रन्थ आदि धार्मिक विषय। इसके पश्चात् आप अपने सदन के भीतर एवं बाहर इन सब विषयों का संग कर सकते हैं और बाहर भी पुष्प, पक्षी, विस्तृत वृक्ष, वन, निर्मल आकाश और आपके आदर्श सहित मेघ के साथ आप सदा उस प्रभु के भाव को धारण किये हुए अनुभव कर सकते हैं। आपको सदा यही अनुभूति होती है कि उसकी विद्यमानता में ही आप विचरण कर रहे हैं और उसके साथ ही आप चल रहे हैं और सम्भाषण कर रहे हैं। आप स्वयं को उसका पुत्र अथवा पुत्री, सहायी अथवा मित्र मान सकते हैं। स्वयं को उसका सेवक भी मान सकते हैं। उससे आप आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो उससे वार्तालाप कर सकते हैं। आप कुछ भी करें, उससे सम्बद्ध हों-वह चाहे उन्नत (उत्कृष्ट) हो अथवा विरस, उत्साहवर्धक हो अथवा दुष्कर एवं समस्यायुक्त। आप दिन-प्रतिदिन, क्षण-प्रतिक्षण यत्किंचिदपि कर रहे हो, वह सब उसके अर्पण करो। यदि कोई उपहास भी करो, तो प्रभु के साथ भागी बनो। कुछ असाध्य हो तो उससे पूछो-"अब मैं क्या करूँ?" भयग्रस्त हों तो उससे कहो-"अब तुम्हीं मेरा साहस हो।" दुर्बलता अनुभव करें तो कहें- "हे प्रभु, मुझे शक्ति दो!" यदि आप कोई भूल करें तो कहें- "हे प्रभु, मुझे क्षमादान दो!" इस प्रकार सदा उससे सम्पर्क बनाये रखो। आध्यात्मिक कल्पना में ऐसा सम्पर्क स्थापित करने से आप उसके साथ विकसित होते हैं। सतत स्मरण में कल्पना सहायी हो सकती है।
यदि आप अधिक भावुक नहीं हैं, इस प्रकार के भावुक सम्बन्ध की सन्निधि की कल्पना नहीं कर सकते और साथ ही यदि आपको शुद्ध रूप से बाह्य विधि रुचिकर न हो, तो बुद्धि को इस प्रक्रिया में संलग्न करो। यदि आप स्वभाव से दार्शनिक हैं, तो आपकी मेधा-शक्ति ही आपको ज्ञान देगी कि वह सर्वव्यापक सत्ता है। वह सर्वत्र है, आपके अन्तःकरण का अन्तस्तम कोष है। वह आपके अस्तित्व की सारभूत सत्ता है। उसकी सत्ता से ही आपका अस्तित्व है। बौद्धिक क्रम से ही आप कुछ मानसिक धारणाएँ विकसित करते हैं। इस सृष्टि में सब वस्तुओं के पीछे कारण है। कुर्सी का बढ़ई है, जूते का मोची है, वस्त्र की वस्त्र-निर्माण फैक्टरी है और ब्रह्माण्ड में आपके परिवेश में जो तत्त्व हैं, उनका भी निर्माता है। ब्रह्माण्ड किसी महान् कारण से उद्भूत कार्यस्वरूप है। आप जब जगत् की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो आपकी बुद्धि ही आपको सूचित करती है कि इसके पीछे एक मूल कारण होगा। इस प्रकार इन बौद्धिक प्रक्रियाओं से आप उसकी अनुभूति का प्रयास कर सकते हैं।
ब्रह्माण्ड का गौरव देखो। इसके मूल कारण सर्वव्यापक सत्ता का गौरव कितना अधिक होगा? वह अनिर्वचनीय है। वह सर्वव्यापक है। इस प्रकार की विवेकपूर्ण धारणाओं से उसकी विद्यमानता को अनुभव करने का यत्न करो। उसे सब कारणों का मूल कारण रूप, सब पदार्थों में व्यापक और सबकी पुष्टिदायक अविभाज्य सत्ता जानो । उसे अपने अन्तःकरण के अन्तस्तम गर्भ के रूप में अवलोकन करने का प्रयास करो जिसने आपको जीवन प्रदान किया है। वह आपके जीवन का जीवन है। वह आपकी सत्ता का सार है। आपके अस्तित्व का आधार है। यदि आप सदा और सर्वत्र इस प्रकार का अभ्यास करें, तो जिस क्षण आप ध्यान हेतु आसनस्थ होंगे, विक्षिप्त रूप लेने वाला ध्यान अब प्रगाढ़ रूप धारण करेगा। इसी का अभ्यास करो।
आपको बतायी गयी सतत स्मरण की ये विधियाँ पाश्चात्य रहस्यवादियों की हैं। पूर्वीय आचार्यों ने एक अन्य विधि निर्दिष्ट की है। वे अनवरत नाम-जप का आदेश देते हैं-वह चाहे शाब्दिक हो, जपाजप (जिसमें केवल ओष्ठ हिर्ले, पर स्वर न हो) अथवा मानसिक जप हो। यह अभ्यास भी आपको भगवद्-चिन्तन में संलग्न रखता है। यह किसी दिव्य नाम का जप अथवा कोई लघु सूत्र अथवा प्रार्थना हो सकती है। यह लघु एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। यही इसका सार है। आप कह सकते हैं- "हे प्रभु! मैं आपकी स्तुति करता हूँ। है ईश्वर, मैं आपका ही गुणगान करता हूँ।" अथवा, "कृपा-वृष्टि करो, प्रभु आपकी जय हो।" अथवा, "भगवान्! आपकी जय हो!" अथवा "मैं आपसे स्नेह करता हूँ।" अथवा, "आप मेरा ध्यान करें, प्रभु आप मुझे विस्मृत न करें, मुझे विस्मृत न करें।" अथवा, "मैं सर्वदा आपके साथ हूँ।" इस प्रकार से जप का अभ्यास करते रहें। उस प्रभु का आह्वान करने के लिए कतिपय शब्दों का चयन करो। "हे प्रभु, मेरे साथ रहो, प्रभु मेरे साथ रहो, प्रभु सदा ही मेरे साथ रहो।" प्रातः, मध्याह्न एवं सन्ध्या काल के लिए आप पृथक् पृथक् शब्द-समूह ले सकते हैं अथवा उनका क्रम से पर्यायेण परिवर्तन कर सकते हैं। उनका सतत प्रयोग करते हैं जिससे आपके भीतर दिन की प्रत्येक वेला में सम्पूर्ण दिवस पर्यन्त भगवद्-विचार की अटूट धारा बनी रहे अथवा आपको उसकी अनुभूति होती रहे। इसी से वास्तविक सफलता हाथ लगती है। परमात्मा के सतत स्मरण का अभ्यास ही आभ्यन्तर ध्यानस्थ जीवन का आधार है। यह गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
एक यूरोपियन रहस्यवादी सन्त ने कहा है- "जो केवल उसी समय प्रार्थना करता है जब वह घुटने टेक कर बैठा हो, तो वह बहुत कम प्रार्थना करता है" अर्थात जब आपका आन्तरिक जीवन केवल उन्हीं क्षणों में सीमित है जब आप वस्तुतः घुटनों पर हों और शेष समय आपका मन धरातल पर प्रत्येक वस्तु का अनुसरण करते हुए जंगली वानर के समान है, तो आप बहुत कम प्रार्थना करते हैं और तब आपकी प्रार्थना कदापि सशक्त (प्रभावशाली) नहीं हो सकती; क्योंकि शेष समय आपके अन्तःकरण की दशा ध्यानपरक जीवन से सर्वथा विपरीत होगी और इसलिए ध्यान नहीं किया जा सकता। सतत भगवद्-स्मरण का स्वभाव बनाने का प्रयास करो। आभ्यन्तर सत्ता के साथ आपके सम्पर्क का प्रभाव तथा ध्यान में ईश्वर से सान्निध्य का वास्तविक अंश ईश्वर में निरन्तर वास के अंश के अनुपात में होता है जो सम्पूर्ण दिवस पर्यन्त भगवद्-स्मरण द्वारा प्राप्त किया गया हो।
ध्यानार्थ ही हमने मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है। ध्यान ही एकमात्र महत्त्वपूर्ण कार्य है। यथार्थ समन्वय मन की वास्तविक स्थिरता, सच्चा, अखण्ड, साक्षात् व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए यही एकमात्र साधन है। वास्तविक शान्ति और आनन्द की प्राप्ति हेतु यही एक साधन है। मैं अपने भाषण में वैधिक अथवा दृढ़ नहीं बनना चाहता; किन्तु इसके प्रति मैं पूर्णतः वैधिक एवं विश्वस्त हूँ कि सच्ची शान्ति और आनन्द की प्राप्ति हेतु यही एकमात्र साधन है। यदि आप ध्यान त्याग कर अन्य विधियों का अनुष्ठान करें, तो अन्ततः आपको यह कटु अनुभव होगा कि जीवन व्यर्थ खो दिया गया है और तब बहुत विलम्ब हो चुका होगा। तब आप पश्चात्ताप करेंगे - "काश! मैंने पहले ही ध्यान प्रारम्भ किया होता!" ऐसी भूल मत करो। ऐसा अपराध मत करो। जीवन की सभी विविध क्रियाओं में इस महती प्रक्रिया को मानव जीवन की प्रमुख प्रक्रिया को करते चलो। यही ध्यान ही सुख का द्वार है और वास्तविक तथा नित्य शान्ति का एकमात्र साधन है।
आपसे कहा गया है कि आपका समस्त जीवन इस प्रक्रिया का आश्रय होना चाहिए। जीवन की शुद्धता ध्यान के लिए नितान्त आवश्यक है। उस एक पद से मेरा अभिप्राय इन सभी गुणों से युक्त होने से है-पूर्ण सात्त्विक चरित्र, नैतिक जीवन के आदर्शों की पूर्ति, गुणों का संवर्धन, भद्रता में विकास और संक्षेप में जहाँ तक सम्भव हो स्वभाव से देवतुल्य होना। शुद्ध पवित्र मन ही ध्यान कर सकता है। ध्यान में विलम्ब न करो जो आपको सब अशुभ बुराइयों का अतिक्रमण एवं सर्व दोषों का निराकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें स्वभावज शुद्धि प्रवाहित करने की क्षमता है। यह शुद्धि प्रदान करता है। यह आत्मनिष्ठ होने के लिए इन्द्रियों तथा तृष्णा पर प्रभुत्व स्थापित करने तथा परिपूर्ण शुद्धता में विकसित होने के लिए आत्म-शक्ति प्रदान करता है। नित्य अभ्यास द्वारा मनोयोग का अवरोपण करना अनिवार्य है। मनोयोग से एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान में उन्नति का अद्वितीय साधन एकाग्रता है। ईश्वर के लिए आसक्ति का विकास करो। जहाँ आसक्ति है, वहीं मन और हृदय है। अतएव परमात्मा के लिए प्रेम बढ़ाओ।
अन्ततः, इस समय यदि आप घर जायें और निद्रा से पूर्व ध्यान में बैठें, तो इस अभ्यास को प्रतिदिन करते रहें। एक दिन के लिए भी इसका त्याग न करें, आप स्वस्थ अथवा अस्वस्थ, निराश हों अथवा व्याकुल, कुछ भी हों, चिन्ता न करें। यदि आप सबसे महती पूँजी; सब पूँजियों की पूँजी का आलिंगन करें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन में आपके समक्ष कठिनतम समस्या भी आ खड़ी हो, आपको बृहत्तम और उग्रतम वियोग का आघात भी क्यों न सहना पड़े, सर्वोच्च परीक्षा अथवा परीक्षण अथवा प्रलोभन का अनुभव क्यों न करना पड़े-इन सबको ध्यान-शक्ति द्वारा आप अतिक्रमण कर सकते हैं। आप ध्यान द्वारा निजात्मा का सीधा परमात्मा के साथ सम्पर्क स्थापित करते हैं। वह सर्वशक्तियों की शक्ति है। वह सबसे बड़ी शक्ति, महानतम बल और सब सद्गुणों की खान है। वह सब परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। उस शक्ति के द्वारा सर्वातिक्रमण हो सकता है। अन्ततोगत्वा, स्वयं मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।
ध्यान आपको परम लक्ष्य-मृत्युंजय तथा शाश्वत जीवन की प्राप्ति, भगवान् में परम विजय की ओर अग्रसर करे! यही मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है।
ध्यान-सर्वरोगहर औषधि
मध्यकालीन सन्त अलकान्तरा के सेन्ट पीटर ने कहा है ध्यान (मानसिक प्रार्थना) की उपेक्षा करने वाले मनुष्य के लिए निष्पाप रहना नैतिक रूप से सर्वथा असम्भव है। मानसिक प्रार्थना की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति को नरक की ओर आकृष्ट कर ले जाने के लिए दैत्य की आवश्यकता नहीं है, वह अपने ही हाथों से स्वयं को वहाँ ले जाता है। इस कथन को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं कि अन्य साधन में ध्यान के समान अद्वितीय शक्ति नहीं है और परिणामतः इसके अभ्यास का स्थान अन्य विधि नहीं ले सकती। सब सन्तों का सामान्य अभ्यास और महान् धर्माचार्यों के लेख प्रमाण हैं कि ध्यान को जीवन में सर्वोच्च पूजार्ह स्थान देना चाहिए।
ध्यान आपके समस्त व्यक्तित्व के पूर्ण आध्यात्मीकरण की प्रक्रिया है। यह प्रशान्ति, सुख और समृद्धि में रहने की कला है। मन पवित्र होने पर स्वभावतः ही समृद्धि को आकृष्ट करता है। यह व्यभिचार और अमरत्व के अभ्याघात के विरुद्ध मन की परख है। जीवन के सभी धर्मों के लिए ध्यान अतीव अमोघ है। चिन्ता नहीं, आप किस धर्म को मानते हैं; व्यक्तिगत अथवा सामाजिक अपनी उन्नति के हेतु आपको शरीर, मन और आत्मा के समन्वित विकास की आवश्यकता है। ध्यान की इस अखण्ड प्रक्रिया में यह सहसा ही प्राप्त किया जाता है।
ध्यान न केवल जीवन के अन्तः- बाह्य, भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों को अखण्डरूपेण निबद्ध करता है, प्रत्युत आपके अस्तित्व की कान्ति को भी उच्चतर सत्ता अर्थात् अन्तर्निहित ईश्वर की ज्योति से अभिन्न करके उद्दीप्त करता है। अन्ततोगत्वा, यह परिवार और समाज, पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माता-पुत्र, मित्र-मित्र, भाई-बहन, सम्बन्धी और सहकारी, निम्न एवं उच्च, सेवक-स्वामी, व्यवसायी और व्यापारियों के मध्य विरोध (इन्द्र) को समाप्त करने के लिए युक्त साधन है। यह मनुष्य को शान्ति और विवेक से परिपूर्ण करता है।
यह क्या नहीं कर सकता? यह आपके लिए कुछ भी कर सकता है। जीवन में सब दोषों को समाप्त करने के लिए यह सुनिश्चित उपाय है। यह सब पापों को दग्ध करने की अग्नि है। ध्यान-रूपी अग्नि की प्रज्वलित ज्वाला में पापी, पापी नहीं रह सकता। संसार के द्वन्द्वों से अछूते रह कर जीने की कला ध्यान है। ध्यान अप्रभावित कर्म-बन्धन से अप्रभावित रह कर जीने का ढंग सिखाता है। शरीर में रहते हुए, जीवन्मुक्ति ही इसका परिणाम है। अतः अत्यन्त गम्भीरता से मैं आपको ध्यान-प्रक्रिया में निमग्न होने का आदेश देता हूँ!
आओ, हम सब मिल कर प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें शक्ति दें जिससे हम स्वयं को पवित्र, सात्त्विक, निःस्वार्थ एवं सेवापरायण जीवन द्वारा प्रभु के प्रति भक्ति विकसित करके और भौतिक तथा ब्रह्माण्ड की संज्ञा वाले रूपों की क्षणभंगुरता और गमनशीलता की शून्यता का आभास करके, अनुपमेय गौरव तथा हमारी सत्ता के आत्यन्तिक स्रोत ईश्वर की अमोघ मूल्यता का अनुभव करके शरीर की स्थिर मुद्रा एवं प्राणायाम की सहायता से मनोनिग्रह एकाग्रता का अभ्यास करके तथा अनवरत नाम-स्मरण का अभ्यास एवं प्रभु की अहेतुकी कृपा-वृष्टि द्वारा ध्यानस्थ होने के लिए स्वयं को तैयार करें। एवंविध हम शनैः शनैः शुद्ध ध्यान की उच्च से उच्चतर अवस्था को पहुँचें और प्रार्थना द्वारा आकृष्ट प्रभु-कृपा से हम अचिरेण ध्यान की उस अवस्था को प्राप्त करें जो हमें भगवद्-दर्शन के सर्वोच्च अलौकिक धाम को ले जाये और हमारे जीवन को आत्मबोध एवं अमरत्व को गौरवमयी उपलब्धि से सुशोभित करे।
आप सब पर प्रभु की कृपा-दृष्टि बनी रहे! एकाग्रता और ध्यान के अन्तःपथ पर दृढ़तापूर्वक चलते हुए पग-पग पर सर्व गुरुजनों एवं सन्तों का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, उनकी सहायता आपको सदा उपलब्ध हो ! प्रभु की अपार कृपा से आप स्व जीवन को प्रशस्त करें!
१५. साधु-सन्त
ज्योतिर्मय अमर आत्मन्! परमात्मा की गौरवशाली सन्तान! प्रिय जिज्ञासु गण! आपके पुण्य तेज में निमज्जन का सौभाग्य प्राप्त करके मुझे अतीव हर्ष और आनन्द की अनुभूति हो रही है। भारत में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा जिस वस्तु से परमानन्द प्राप्त कर सकती है, वह है प्रभु-प्रेमियों की संगति! अनेक वस्तुएँ उपलब्ध की जा सकती हैं-आप अमूल्य धन-सम्पत्ति और भौतिक पदार्थों के स्वामी हो सकते हैं; किन्तु शुद्ध हृदय प्रभु-प्रेमी सत्यान्वेषियों की संगति के समक्ष ये सब तुच्छ हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता। यह तो हमें उस प्रभु की अहेतुकी कृपा से ही प्राप्त होती है। यह वरदान है जो सीधा प्रभु से प्राप्त होता है। दिव्य स्वरूप परमात्मा जब हम पर कृपा-वृष्टि करना चाहते हैं, तब इसका आगम होता है। इस दृष्टि से वह हम पर अत्यन्त कृपालु हैं। लोग पश्चिम के निष्ठा-रहित, नास्तिक, आधुनिक युग की बात करते हैं; किन्तु गत डेढ़ वर्ष में मैंने तो केवल आध्यात्मिक पश्चिम में विचरण किया है। मैंने भौतिकवादी पाश्चात्य देश का दर्शन नहीं किया। भगवद्-प्रेमियों के परिसर में वास करने वालों के लिए यह स्वर्णिम युग है। आप किसी भी युग में रहें, चिन्ता नहीं। जिन प्रभु-भक्तों, सत्यान्वेषियों और जिज्ञासुओं ने यह अनुभव कर लिया है कि जीवन गमनशील, परिवर्तनशील है और असत्यता में व्यर्थ गँवाने के लिए नहीं है, प्रत्युत उत्कृष्ट क्रम-भगवद्-साक्षात्कार- हित है, ऐसे सद्पुरुषों की संगति में आना ही स्वर्णिम युग में प्रविष्ट होना है। वह मनुष्य वस्तुतः धन्य है जो सत्संगति में रहता है।
सन्तों की पवित्रीकरणी शक्ति
सत्संग रूपान्तरक है। उन लोगों के संग को सत्संग कहते हैं जो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ अभिन्न रूप हैं। 'सत्' परम सत्य अथवा वास्तविकता का बोध कराता है। 'संग' का अर्थ है 'साथ' । सत्संग का अर्थ है परमात्मा की सन्निधि। सर्वोत्कृष्ट अथवा पुण्य संग है-ईश्वर के साथ रहना, भगवद्-चिन्तन, दिव्य भावना, ध्यान अथवा आराधना में रहना । इन प्रक्रियाओं की सहायता से आप सच्चिदानन्द की सन्निधि प्राप्त कर सकते हैं।
भूतल पर दिव्यता की साक्षात् अनुभूति महान् भ्रातृरूप साधु-सन्तों, पुण्यात्माओं और भक्तों में अवलोकित होती है। ईश्वर ने कहा- “वह पृथ्वी तीर्थ-स्थल है जहाँ मेरे भक्तों का वास है।" यह समस्त धरती पवित्र है। जिन पावन स्थलों पर जनगण परमानन्द की प्राप्ति हेतु तीर्थ करने जाते हैं, उन स्थलों की पवित्रता इन भक्तों की विद्यमानता से होती है। भक्त जनों ने वहाँ जा कर भगवान् की आराधना की और भगवद्-साक्षात्कार किया, इसलिए वे स्थान तीर्थ-स्थल बन गये। यह सब इसलिए नहीं कि भक्त वहाँ गये; क्योंकि स्थान पवित्र थे, प्रत्युत भक्तों के वहाँ गमन से स्थान पवित्र हो गये। संसार में पुण्यात्मा और सन्तगण पवित्रीकरणी शक्तियाँ हैं। इन सन्तों के कारण ही विश्व रहने योग्य स्थान बन जाता है। सन्त एक महान् आदर्श के प्रतीक हैं। अनुभव-विशेष के कारण वे तेज से भासित होते हैं।
प्राचीन भारतीय प्रथा के अनुसार गंगा एक पावन नदी है, दिव्य धारा प्रवाह है जिसमें स्नान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगा पापों को किस विधि प्रक्षालित करती है? किसी ने माँ गंगा से कहा- "पार्थिव जीवन की एक ही अवधि में मनुष्य जो पाप और अशुद्धताएँ समवेत करता है, उनसे मुक्त होने के लिए उसे पर्याप्त तपश्चर्या, प्रार्थना, तीर्थ, आध्यात्मिक अनुष्ठान और आराधना करनी पड़ती है; किन्तु हे माँ गंगा, तुम अपने ऊपर कोटि-कोटि लोगों की असंख्य बुराइयाँ और पाप धारण करती हो। हे माँ! पुनरपि तुम सर्वशः पवित्र नदी मानी जाती हो, इसका रहस्य क्या है?"
ऐसी जन-श्रुति है कि माँ गंगा ने उत्तर दिया- "यदि एक कोटि पापी मुझमें स्नान करके मुझे अपवित्र करते हैं और तदुपरान्त यदि एक सन्त आ कर मुझमें निमज्जन करता है, तो मैं तत्काल पवित्र हो जाती हूँ। कोटि जनों के सर्व पाप लुप्त हो जाते हैं; क्योंकि सन्त की सर्वग्राह्य प्रकृति के कारण उसके निमज्जन मात्र से पूर्व की सर्व अशुद्धताएँ घुल जाती हैं, उनका लोप हो जाता है।" ऐसे लोगों की संगति, उनके जीवन का मनन, सन्तों का विचार मानो एक नदी है जिसमें गोता लगाया जाये, निमज्जन किया जाये और यह निमज्जन गंगा स्नान से सहस्रगुणा अधिक पवित्र करने की शक्ति रखता है; क्योंकि गंगा स्वयं सन्तों के द्वारा ही पवित्र होती है।
सन्त शाश्वत सत्यों के साक्षी स्वरूप हैं। संसार के अस्तित्व को मानना सुगम है; क्योंकि यह दृष्टिगोचर है। जो संसार हमारे समक्ष विद्यमान है और जिसे प्रतिज्ञान चाहिए, इसके सर्व अनुभव किसी-न-किसी इन्द्रिय द्वारा प्राप्त होते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि संसार नहीं है। दूसरी ओर अदृश्य तो अधिकांश जनपद के लिए मात्र विचारणा है जब तक कि शाश्वत सत्ता में मनुष्य उद्दीपक श्रद्धा का अनुभव नहीं करने लगता। और साधु-सन्त जिन्होंने स्वयं ही अपने अद्भुत जीवन में भगवान् की असीम सत्यता का साक्षात्कार किया, जो महान् हैं, शाश्वत हैं, वे मानो परमात्मा के अस्तित्व के अनिवार्य तथा अनिगृहीत साक्षी हैं।
यदि आपसे प्रश्न किया जाये- "आप भगवान् में विश्वास क्यों करते हैं?" आप केवल यही कह सकते हैं- "क्योंकि सन्त विद्यमान हैं, क्योंकि वे भगवद्- स्वरूप हैं।" आप पुत्र को देख कर पिता की सत्ता को अंगीकार करते हैं। इसी प्रकार से सन्तों के दर्शन से आपको असीम आनन्द और शान्ति के स्रोत का ज्ञान होता है; क्योंकि सन्तों में साक्षात् रूप से आप उस पूर्वकालिक शान्ति के दर्शन करते हैं। सन्त उस आभ्यन्तर शान्ति से परिपूर्ण होते हैं जो किसी विषय से प्राप्त नहीं की जा सकती। एक विरक्त संन्यासी जिसका वासस्थान कदाचित् किसी पर्वत-गुहा अथवा नदी-तट पर हो, जिसके पास कोई पार्थिव सम्पत्ति न हो, पुनरपि वह एक अलौकिक आनन्द की आभा से भासित होता है और कोई भी उससे उस आनन्द को छीन नहीं सकता। प्रत्युत व्याकुल, अशान्त और सन्तप्त लोग उसकी सन्निधि में शान्ति प्राप्त करते हैं। उससे शान्ति किस प्रकार आती है? क्योंकि उसने सर्वशान्ति और आनन्द के अप्रमेय स्रोत को दिव्यानुभूति द्वारा खोज लिया है। इसलिए सन्तों का मात्र अस्तित्व भी परमात्मा के संसार के अस्तित्व में विश्वास का प्रमाण है।
शास्त्रों और मतों के परस्पर विरोधी वचन
परम तत्त्व की ओर जाने का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा है और विरोधी वचनों से यह सम्भ्रान्तिपूर्ण हो जाता है। विशेषतया इस आधुनिक युग में मनुष्य धर्म के सम्बन्ध में सम्भ्रान्त है। वह नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, वास्तविक धर्म क्या है। विभिन्न धर्मों में विश्वास की अधिकता है। अनेक धर्मशास्त्र हैं जो अपने-अपने ढंग से परम सत्य के प्रति परस्पर विरोधी वचन कहते हैं। उनमें परस्पर मतभेद हैं। एकमत नहीं है और प्रत्येक धर्म अपने मत को ही परमात्मा तक पहुँचाने का एकमात्र सच्चा पथ घोषित करता है। कभी-कभी तो वे इस पर भी नहीं रुकते, प्रत्युत एक पग और आगे बढ़ते हैं-"अन्य सब धर्म आपको नरक की अग्नि में धकेलेंगे और आपको उसी दशा में, शताब्दियों पर्यन्त नरक के अग्निकुण्ड और गन्धक में वास करना होगा। जो इसमें विश्वास नहीं करते, वे सब देव-प्रतिमा-पूजक और उपासक हैं।"
मुसलमान कहेगा- "जो अल्लाह में विश्वास करता है, वही सुरक्षित है। यही एक पथ है जिस पर चल कर स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यही एकमात्र साधन है।" वह अन्तिम लक्ष्य क्या है? यह अक्षय्य स्रोतों, झरनों और कठिनाइयों की भूमि है जहाँ सर्वत्र सुन्दर फल-फूल लगे हुए हैं और स्वस्थ टर्की पक्षी, शुक तथा क्रीड़ा करते हुए अन्य पक्षी गण हैं। यह स्वर्ग के प्रति धारणा है। जहाँ सब प्रकार के सुख तत्काल उपलब्ध होते हैं, जब कि गिरजाघर में प्रार्थना करते हुए एक ईसाई भक्त का हृदय सम्पूर्ण संसार के भार से द्रवित हो उठता है। वह आश्चर्य करता है कि किस विधि से वह ईसा के विपथगामी आत्माओं की रक्षा कर सकता है। उसे विश्वास है कि भगवान् के प्रति उसके मत-विशेष में श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए ही आशा की जा सकती है और अन्य सभी के लिए तो अश्श्रु बहाने चाहिए; क्योंकि वे सब देव-प्रतिमा-पूजक हैं, उपासक हैं, जो निजात्मा की रक्षा चाहते हैं। और यदि ईसाइयों ने उनका उद्धार न किया, तो सदा के लिए उनका नरक वास होगा। अतः बहुधा एक ईसाईमतावलम्बी सोचता है कि अन्य आत्माओं का उद्धार करना उसका कर्तव्य है और जितना अधिक वह उद्धार करेगा, उतना अधिक उसका अपना मोक्ष निश्चित होता जायेगा।
मुस्लिम और ईसाई दोनों के मतावलम्बियों की यह अपनी-अपनी धारणा है कि उनका धर्म ही एकमात्र धर्म है तथा अन्य सब लोग अन्धे हैं। इसी प्रकार से बौद्ध कहेंगे-"निर्वाण की ओर ले जाने वाले पथानुगामियों की रक्षा करो, अन्य सब तो अन्धकार में निरूपण करते हुए बालक हैं।"
इस प्रकार देखा जाता है कि मत-विरोध है, स्मृति-भेद है, नीतियों में मतभेद है, दिव्यता की धारणा में मतभेद है और इनमें केवल भेद ही नहीं, वे सब परस्पर विरोधी और व्यावर्तक हैं। एक ही धर्म में विभिन्न मतों की सत्यता को दर्शाने की विधि पृथक् है और प्रत्येक मत लड़ने को तैयार है और कहता है कि 'अन्य सभी मूर्ख हैं और केवल उनके पास ही सर्वोच्च सत्य विद्यमान है और वे सभी सच्चे साधक हैं', किन्तु वे अन्य धर्मों का आदर करना नहीं जानते हैं और इसके विपरीत यह सोचते हैं कि अन्य धर्मों के अनुयायी मिथ्या धारणा से युक्त अन्धकार में पड़े हुए हैं। एवंविध प्रत्येक पृथक् धर्मानुयायी अन्य सभी धर्मावलम्बियों की अज्ञानता को घोषित करता है। येन केन प्रकारेण अपने जीवन का उद्धार करके परमानन्द की प्राप्ति की आकांक्षा करने वाला एक सामान्य व्यक्ति सम्भ्रान्त हो जाता है और यह विवेक नहीं कर सकता कि किस धर्म में विश्वास किया जाये। जेट विमान के आज के युग में सब धर्मों का ज्ञान सहज सुलभ है, पुस्तकालयों में रखी पुस्तकों द्वारा जितना अधिक मनुष्य अध्ययन द्वारा ज्ञान-प्राप्ति करता है, उतना अधिक वह भ्रम में पड़ता है। तथापि विरोध, भ्रम और उत्सुकता का मार्ग इस युग की विशेषता नहीं है।
भारत में एक प्राचीन उक्ति है- "वेद और उपनिषद् जैसे प्राचीन शास्त्र भी अपनी-अपनी व्याख्या में भिन्न-मत हैं। भगवद्गीता और महाभारत जैसे शास्त्र का भी जीवन के प्रति तथा आत्यन्तिक सत्य एवं मनुष्य के कर्तव्य के प्रति पृथक् पृथक् विचार तथा व्याख्या 31 ^ 11 आप यदि विविध महात्माओं के लेख पढ़ें, तो वाल्मीकि किसी विषय पर कुछ लिखते हैं तो वसिष्ठ कुछ और लिखते हैं और इसी प्रकार महात्मा बुद्ध तथा अन्य सन्तों की विचारधारा परस्पर एक नहीं हैं।
एक सन्त कहते हैं-"केवल प्रेम के पथ में ही भगवद्-साक्षात्कार सम्भव है। उस परमात्मा के प्रति प्रेम-भाव, उसकी पूजा-आराधना के बिना सर्वस्व व्यर्थ है। ज्ञान कभी मोक्ष नहीं दे सकता। भगवद्-प्रेमी ही प्रभु की कृपा से आनन्द और मोक्ष की परमावस्था को प्राप्त होता है।" अब शंकराचार्य कहते हैं-"ईश्वरीय ज्ञान के बिना मोक्ष का स्वप्न भी असम्भव है। ज्ञान ही वह आत्यन्तिक अग्नि है जो सर्वपापों और संचित कर्मों को दग्ध करके आपको मोक्ष प्रदान करती है। एक सहस्र जन्मों पर्यन्त भी, सर्व प्रकार की पूजा करने, घण्टी बजाने, तीर्थ करने, दान देने, कीर्तन करने से भी ब्रह्मज्ञान के बिना मोक्ष की आशा नहीं की जा सकती।" अन्य सन्तों का कहना है-"मानवता की सेवा, परोपकार, अनवरत सेवा द्वारा ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। केवल अपने लिए मोक्ष की आकांक्षा करना स्वार्थ की पराकाष्ठा है। इस प्रकार से आप इहलौकिक बन्धन कदापि नहीं तोड़ सकते ।''
इन साधु-सन्तों के विचार पृथक् पृथक् हैं। अतएव सात्त्विक जीवन का सात्त्विक सार तथा कर्तव्य का सच्चा भाव प्रायः किसी ऐसे स्थान पर प्रच्छन्न रखा है जो पहुँच से परे है। इसलिए हम पूछते हैं-"पथ कौन-सा है?" वही एक पथ है जिस पथ का महान् आत्माओं ने अनुसरण किया है।
सन्तों के जीवन से अमोघ मार्ग-दर्शन
अतः आप धर्मशास्त्रों की शरण में जा कर कहीं भ्रम में न पड़ जाओ, इसीलिए उस पथ की ओर देखो जिसका अनुसरण इन महात्माओं ने किया है। इन सन्तों के जीवन पर दृष्टिपात करो कि किस प्रकार से इन्होंने परमानुभूति हेतु स्वयं को योग्य बनाया। वे किस विधि बोले, अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, जीवन तथा इसकी अभिव्यक्ति के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? देखो! अपने जीवन को सन्तों के आदर्श के अनुरूप बनाओ और इस प्रकार हमारे लिए सन्तों के जीवन की महानता यही है कि वे हमारे समक्ष अपने सम्पूर्ण जीवन को साक्षात् रूप में उपस्थित करते हैं। उनके जीवन हमारे समक्ष निजी श्लाघ्य व्यक्तित्व को उज्ज्वल करते हुए, अपने जीवन का आदर्श स्थापित करते हुए जीवन की स्पर्शवेद्य प्रयुक्ति, जीवन का ढंग प्रस्तुत करते हैं। हम अनुभव करने लगते हैं कि अब हम सुरक्षित हाथों में हैं और हम केवल उनके चरण-चिह्नों का अनुसरण कर सकते हैं। महान् आत्माओं के जीवन प्रायः हमें स्मरण कराते हैं-काल की मरुभूमि में वे अपने पीछे पद-चिह्न छोड़ जाते हैं और वे 'चरण-चिह्न' अर्थात् उनके जीवन की उपमा हमारे लिए पूर्णत्व के पथ के लिए पथप्रदर्शक बन जाती है।
आइए, हम सिद्धान्त, मत, नीति और विभिन्न धार्मिक गुटों के बृहत् चक्र से बचते हुए महान् सन्तों के पद-चिह्नों का अनुसरण करें। हमें अध्यात्मवादी धारणाएँ ब्रह्मज्ञानियों के हाथ में सुरक्षित छोड़ देनी चाहिए; क्योंकि वे इहलौकिक पदार्थों से सम्बद्ध हैं। वरंच हमें ब्रह्म-विद्या के हद्देश में उतर कर, इसके सार को जान कर उस पथ पर अनुसरण का प्रयास करना चाहिए जिस पथ से हमारे सन्त गण गये हैं। यदि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सन्तों का कोई स्थान है, तो हमें उनकी प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। हमें उनकी भाँति जीवन-यापन करने का अभ्यास करना चाहिए, उनके समान अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए, उनके जीवन को अपने चरित्र का एक स्तर, मानदण्ड बना लेना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में, जिसमें हम कर्म के विवेक से अनभिज्ञ हैं, हमें स्वयं को कहना चाहिए- "इस परिस्थिति में अमुक सन्त ने किस प्रकार आचरण किया होगा?" अथवा, "यदि मेरे स्थान पर सेंट फ्रांसिस होते, तो वे कैसा आचरण करते? यदि ईसा मसीह को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता तो उन्होंने क्या किया होता? यदि राम और बुद्ध इस परिस्थिति में होते, तो उन्होंने क्या किया होता?"
आप निजात्मा से उच्च स्तर की अभिलाषा नहीं कर सकते; किन्तु स्तर न रखने अथवा निम्न और तुच्छ स्तर रखने से तो उच्च स्तर धारण करके उसमें असफल होना अधिक अच्छा है। सन्तों के जीवन इस बात का प्रमाण हैं कि यदि मनुष्य में पर्याप्त इच्छा-शक्ति हो, तो वह सर्वस्व प्राप्त कर सकता है।
महान् सन्तों के जीवन का अध्ययन करो। आपको ज्ञात होगा कि उनका जीवन भी कैसे छिद्र से प्रारम्भ हुआ, सामान्य जनपद की भाँति वे भी प्रारम्भिक काल में किस प्रकार दुर्बलताओं और दोषों से पूर्ण और विनम्र थे। किन्तु किसी आदर्श के प्रेम से प्रभावित हो कर अपनी जिज्ञासा, निष्कपट भाव और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, उस आदर्श का अनुगमन करने में अपने दृढ़ निश्चय द्वारा संसार की आक्रामक वृत्ति तथा इस प्रक्रिया में अनुभव, अनेक विघ्नों और समस्याओं का सामना करने की चिन्ता न करते हुए उन्होंने विजयश्री प्राप्त की। उनकी समस्याएँ और कष्ट ही ऐसे तथ्य सिद्ध हुए जिनसे उनकी प्रकृति निर्मल हुई और उनकी सम्पूर्ण मलिनता दूर हुई तथा वे शुद्ध स्वर्ण की भाँति कान्तिमान हो कर चमकने लगे। जीवन उनके लिए एक अग्निकुण्ड बन गया जो तुच्छ खनिजधातु को शुद्ध करके इसे शुद्ध प्रभासित स्वर्ण में परिणत करता है। इस प्रकार सन्तों ने हमें दर्शाया है कि कोई भी सर्वसामान्य व्यक्ति वही कार्य कर सकता है जो उन्होंने किया।
इस प्रकार उनके जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा-स्रोत बन जाते हैं। उनके जीवन की विशद घटनाएँ महान् साहस और प्रज्ञा के स्रोत हैं। उनका जीवन पढ़ते हुए ऐसा आभास होता है मानो हमारे पास साक्षात् ज्ञान आ गया हो। इन महान् सन्तों के जीवन का चिन्तन करने से निराशा के क्षणों में हमें साहस मिलता है। अतएव सन्त गण इस पथ के मौलिक दृष्टान्त हैं। भगवान् ने हमें सन्त दिये हैं जिससे हम अपने समक्ष पूर्णत्व की प्रतिमूर्ति और आदर्श रख सकें जिसमें हमें स्वयं को ढालना है और उनकी भाँति पूर्ण रूप से सुसंस्कृत होना है। उनके पद-चिह्नों का अनुगमन करके, उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ को अपना कर हम प्रशान्ति और आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। क्या थॉमस ए कैम्पिस द्वारा अपनी कृति को दिया गया शीर्षक "ईसामसीह का अनुकरण" अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है? ईसा का जीवन अनुकरणीय है। हमें वही बनना है जो वह थे। हमें महान् आत्माओं, सन्तों और रहस्यवादियों जैसा बनना है। वे आदर्श स्तर प्रदान करते हुए प्रेरणा के अक्षय्य स्रोत हैं जिन पर हमें अपना जीवन आधारित करना चाहिए। ये सन्त पुण्य ग्रन्थों की सजीव प्रतिमूर्ति हैं। धर्मशास्त्रों के सब उत्कृष्ट उपदेश, महान् सत्य, इन साधु-सन्तों के जीवन, वचनों तथा कर्मों में प्रकट-रूपेण दृष्टिगत होते हैं। पुस्तक के रूप में धर्मशास्त्र ज्ञान का भण्डार हैं, किन्तु सन्तों के जीवन पर दृष्टिपात करने से हम शास्त्रों के सत्य की सजीव शक्ति और साक्षात् सत्य के रूप में अवलोकन करते हैं। अतः सन्तों से हम प्रेरणा, महती आशा और साहस प्राप्त करते हैं। हमें पूर्णत्व की उस अवस्था की ओर संकेत मिलता है जिसमें हमें स्वयं को उत्थित करना है, अपना विकास करना है और हम जीवन के एक निश्चित आदर्श स्वरूप और अस्तित्व को प्राप्त करते हैं जो हमें सहज सुलभ होता है।
श्रीमद्भगवद्गीता के द्वादश अध्याय में अर्जुन को उपदिष्ट योग पर अपने संक्षिप्त संवाद की इतिश्री करते हुए भगवान् कृष्ण अन्तिम अष्ट श्लोकों में ब्रह्म को आत्म-समर्पण करने वाले व्यक्ति के आदर्श और उसके जीवन के बारे में बतलाते हैं। यह अनुसरण करने योग्य सुन्दर आदर्श है।
इन महान् सन्तों, रहस्यवादियों, तत्त्वज्ञानियों की विद्यमानता हमें पदार्थों के सर्वथा पृथक् मूल्यांकन का उपदेश देती है। उनके जीवन में हम देखते हैं कि शेष संसार के साथ बहुधा उनकी क्रियाएँ अत्यन्त विस्मय-विमुग्ध करने वाली तथा सन्दर्भ से भिन्न एवं विषम होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे संसार के विधान के विपरीत चल रहे हैं, विशेषतया मौलिक रूप में। किन्तु यदि आप मूल के नीचे खोज करें, तो आपको ज्ञात होगा कि उनके पास अपने चरित्र के अनन्य आचार-व्यवहार के लिए गहनतम ज्ञान-शक्ति है। सन्त कहते हैं-"आप कुछ विशेष पदार्थों के पीछे लगे हुए हैं जो आपको आवश्यक प्रतीत होते हैं, अतः आप अपने ही ढंग से उनका अनुगमन कर रहे हैं। हम उन पदार्थों के पीछे लगे हैं जो हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक और अमोघ हैं और हम अपने ढंग से उनकी प्राप्ति में साधन-रत हैं।"
सन्तों की दृष्टि भी सर्वथा अनन्य हुआ करती है। संसारी मानव की दृष्टि "मैं” और "मेरे" के रंग में रँगी होती है। वह पार्थिव वस्तुओं का आलिंगन करता है। सन्तों की दृष्टि में तो "मेरा नहीं" के भाव का रंग चढ़ा होता है। वह अनुभव करते हैं कि शरीर सहित प्रत्येक वस्तु उस प्रभु की है, उनकी निजी नहीं।
सन्त में रूपान्तरण-शक्ति
बिहार राज्य में गंगा के तट पर एक साधु का वास था जो वेदान्ती किन्तु राम-भक्त था। वह अनेक वर्षों से एक गुफा में योगाभ्यास कर रहा था जो उसने नदी-तट पर स्वयं ही बनायी थी। वह उत्कृष्ट आध्यात्मिक अवस्था को पहुँच चुका था। वह अनेक दिवस, सप्ताह पर्यन्त समाधि में लीन हो जाता और उस अवधि में भोजन ग्रहण न करता। इस कारण से वह पवनाहारी महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राम-भक्त होने के कारण उसके पास पूजा की पर्याप्त सामग्री थी जैसे-बर्तन, तश्तरी, पात्र, चम्मच, प्रदीप एवं मोमबत्ती। भक्त गण आते और उन्हें मुक्तहस्त से फल, पुष्प, कपूर और धूप अर्पण करते और वे इन पदार्थों को भगवान् को अर्पण कर देते।
एक रात्रि को एक चोर उनकी गुफा में आ गया। उसे ज्ञात था कि यह महात्मा भगवान् का भक्त है और निःसन्देह इसने अपने भक्तों से पर्याप्त राशि अर्जित की होगी। चोर अपने साथ एक बोरी भी ले आया था। उसने सन्त की अनेक मूल्यवान् वस्तुएँ उस बोरी में डाल लीं। सन्त भीतरी गुफा में थे। आगन्तुक की ध्वनि पा कर वे बाहर देखने आये कि वहाँ कौन है। सन्त को खड़ा देख कर चोर अपनी बोरी को वहीं फर्श पर छोड़ कर भाग खड़ा हुआ। सन्त ने बोरी उठायी और चोर का अनुगमन किया। उसका अतिक्रमण करके सन्त ने उसे बोरी अर्पित करते हुए कहा- "यह लो, यह तुम्हारी है। तुम भाग क्यों रहे हो? तुमने आ कर इन पदार्थों को एकत्र करने में बहुत कष्ट किया है; अतः बोरी ले लो। तुमने कुछ वस्तुएँ छोड़ दी थीं, वे भी मैंने इसमें डाल दी हैं।" चोर अत्यन्त चकित हुआ। उसे नहीं सूझा कि उत्तर क्या दे। उसने बोरी ली और चल दिया।
कुछ वर्षों के पश्चात् श्री रामकृष्ण के मेधावी शिष्य वेदान्तकेसरी स्वामी विवेकानन्द, जिन्होंने पश्चिम में वेदान्त का सन्देश प्रस्तुत किया, हिमालय-प्रदेश में बदरी-केदार की यात्रा पर थे। उन्होंने एक पुण्यात्मा साधु को ध्यानरत देखा जो वस्त्रों के अभाव के कारण शीत से ठिठुर रहा था। स्वामी विवेकानन्द उससे संलाप करने को रुके और उसे अपना कम्बल ओढ़ा दिया। विवेकानन्द ने अपनी यात्रा एवं मिलने वाले व्यक्तियों का विवरण दिया। उस व्यक्ति ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि क्या वे पवनाहारी सन्त से परिचित हैं? इस पर स्वामी जी ने कहा कि कुछ समय पूर्व ही उन्होंने उस सन्त के साथ कुछ दिन व्यतीत किये। तब उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानन्द से पूछा- "क्या आपने उस चोर के प्रति कुछ सुना जिसने उस सन्त की पूजा की वस्तुएँ चुरायीं और सन्त उस चोर के पीछे उस थैले को ले कर भागे जिसे वह चोर छोड़ आया था और उसमें उन्होंने वे अन्य पदार्थ भी डाल दिये जिन्हें चोर ले न सका था?" स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि उन्होंने उस चोर की कथा सुनी थी। तब वह व्यक्ति स्वामी जी से बोला कि वह ही वही चोर था और उस पवनाहारी महान् सन्त के एक क्षण के सम्पर्क से वह इतना परिष्कृत हो गया कि वह कार्य करके अपनी जीविका अर्जित करने लगा और पश्चात् काल में उसने परब्रह्म की खोज में संसार का भी त्याग कर दिया।
निरभिमानता ही सच्चा साधुत्व है
सन्त गण जिस सिद्धान्त को अपने भीतर सजीव रखते हैं अर्थात् सर्व प्राणियों में भगवद्-दर्शन करना, सबमें आत्म-स्वरूप देखना और कामना रहित पूर्ण अपरिग्रह की अवस्था को प्राप्त करना-यही मोक्ष का द्वार है। अपने भीतर इन सत्यों को वास्तविक रूपेण प्रकट करके हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। और सन्तों की सहनशीलता! साधुत्व का सार ही अभिमान का निराकरण है। संक्षेप में, यदि आप साधुत्व के अन्तःकरण को समवेत करना चाहते हैं, तो अहंकार का सर्वथा नाश करना होगा। वही परम रिक्तता है जिसके विषय में ईसा ने भी कहा - "स्वयं को रिक्त करो, मैं तुम्हें पूर्ण कर दूँगा।" स्वयं को "मैं" और "मेरे पन" के भाव तथा इच्छा, आसक्ति, मोह, क्रोध तथा लालसा रूपी उसकी सन्तान से रिक्त करना है। "मैं" से "मेरा" का उद्भव होता है। "मैं" न हो, तो "मेरा" भी न हो। "मैं" ही वह मूल विचार है जो हमें भगवान् से पृथक् करता है। "मैं" और "मेरा" से स्वार्थ जागृत होता है। "मैं" सर्वस्व ग्रहण कर लेना चाहता है और जीवन में असंख्य इच्छाएँ उत्पन्न होती है। इच्छा-पूर्ति न होने पर क्रोध आता है और यदि इच्छा पूर्ण हो जाये, तो और अधिक इच्छाएँ जागृत होती हैं और इसके उपरान्त लालसा बढ़ती है; क्योंकि इच्छाएँ अतोषणीय हैं, उन्हें शान्त करना दुष्कर है। इच्छा से लोभ अर्थात् इच्छित पदार्थ की प्राप्ति की लालसा उत्पन्न होती है। इस सम्पन्नता से आसक्ति, मोह और भ्रम उत्पन्न होते हैं। सन्त गण इस "मैं" अर्थात् इस अहंभाव से मुक्त रहते हैं।
मेरे गुरुदेव एक मन्त्र गाया करते थे : "स्वयं को सुधारो, परिस्थिति के अनुरूप बदलो, परस्पर मेल रखो, अपमान सहन करो, चोट सहन करो - यही सर्वोच्च साधना है।" अतएव हम सबकी सर्वोच्च साधना अपमान सहन करना, चोट सहन करना है जिसका अभिप्राय है अहंभाव से सर्वथा रिक्त, विनीत-एक शिशुवत् बनना ।
"विनीत चेतस् धन्य हैं। नम्र हृदय वाले जनपद धन्य हैं। आत्मा में निम्न धन्य हैं।" ईसा ने ऐसा क्यों कहा? वे जानते थे कि वे क्या बोल रहे हैं। वे स्वयं अहंभाव से रहित थे। अतः जब उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने अपनी आत्मा की सत्यता से उद्दीप्त शब्द कहे। और जब उन्होंने वे शब्द कहे, वे विनीत थे, नम्र थे और निम्न थे। बालक भी ऐसे होते हैं स्वेच्छित सहजभाव युक्त, निर्दोष एवं निरहंकारी। बालक नम्र हुआ करते हैं। आप एक बच्चे का तिरस्कार नहीं कर सकते। वे निम्न होते हैं, विनीत होते हैं; क्योंकि वे अपनी प्रकृति से विमल, निरपराध और शुद्ध स्वरूप होते हैं। सन्त गण अपने जीवन में इसी पथ का अनुसरण करते हैं।
हमारे समक्ष महाराष्ट्र के महान् सन्त एकनाथ का दृष्टान्त है जो शान्ति, सौम्यता और नम्रता की प्रतिमूर्ति थे। उस स्थान पर अनेक विद्वान् पण्डितों के होते हुए भी उनका प्रवचन श्रवण करने के लिए जनगण की अपार भीड़ उमड़ पड़ती। पण्डित लोग इसे सहन नहीं कर सकते थे। वे उसे अशिक्षित समझते थे और इसलिए उसके पास जनपद का आकर्षण देख कर कुपित होते, क्योंकि अब उनके पास कोई उपदेश लेने अथवा कुछ श्रवण-लाभ हेतु न आता। उन्होंने योजना बनायी कि एकनाथ से कोई ऐसा कार्य करवाया जाये जिससे वे अधीर हो कर क्रोध करें और जनपद को अपनी प्रकृति का दूसरा पक्ष दर्शायें।
उन्होंने एक मनुष्य को वेतन दे कर बुलाया जो वास्तव में धूर्त था। उसे एक स्थान-विशेष पर प्रतीक्षा करने को कहा गया, जहाँ से समाधि में पूजार्थ जल का पात्र लिये वे सन्त पावन गोदावरी नदी में स्नानोपरान्त वहाँ से गुजरते। उस व्यक्ति से कहा गया कि वह मुख में पानी भर कर खड़ा रहे और एकनाथ के आने पर वह उन पर कुल्ला कर दे। हिन्दू के लिए इस प्रकार से किसी के ऊपर थूकना उसे अपवित्र करना है। हाथ भी यदि मुख से स्पर्श कर जाये, तो उसे धोना चाहिए और थूके जाने पर तो समाधि में प्रवेश से पूर्व स्नान अनिवार्य है।
आगामी दिवस एकनाथ नदी पर स्नानार्थ एवं जल ग्रहण करने के लिए गये। जैसे ही वे समाधि में पूजार्थ जाने के लिए नगर के द्वार से जा रहे थे, उस वेतनयुक्त धूर्त व्यक्ति ने उन पर थूक दिया। एकनाथ ने उस व्यक्ति का अवलोकन दिया, अपना मस्तक झुकाया और पुनः स्नान करने के लिए लौट पड़े। ऐसा एक-दो बार नहीं हुआ। १०७ बार ही, जैसे ही एकनाथ स्नानोपरान्त उस द्वार से निकलने लगते, वह धूर्त उन पर धूक देता। बिना एक शब्द कहे और बिना क्रोध, कोप अथवा उत्तेजना दर्शाये वे सन्त लौट जाते और पुनः नदी में स्नान कर आते। १०८ वीं बार जब एकनाथ द्वार पर पहुँचे जहाँ वह धूर्त खड़ा था, उसने ऐसा अभिनय किया मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। वह काँप उठा और स्वयं को धूल में, सन्त के चरणों में गिरा दिया और क्षमा-याचना की। उसने कहा- "मैंने तो सोचा था, मैं मनुष्य से खेल रहा हूँ; किन्तु ज्ञात हुआ आप मनुष्य नहीं देवता हैं।" शेष जीवन के लिए वह धूर्त एकनाथ का सेवक बन गया।
एक सम्राट् के हृदय में पुण्यात्माओं के लिए महान् आदर था। उसके भवन में सदा ऐसे ही महात्मा आते रहते थे। इससे उसके मन्त्री गण क्रुद्ध हुए और एक-दूसरे से बोलने लगे- "हम राजा की सेवा करते हैं, उसे परामर्श देते हैं, उसका राज्य चलाते और युद्धकाल में उसके लिए बलिदान देने को भी उद्यत रहते हैं और यह तुच्छ परिव्राजक, जिनके पास अपना कहने को किंचिदपि नहीं है, राजा के प्रिय प्रतीत होते हैं। राजा हमारी अपेक्षा उनके सुख आदि का अधिक ध्यान करता है।" उन्होंने मुख्यमन्त्री से विचार-विमर्श किया और कहा कि यह सब नहीं होना चाहिए।
मुख्यमन्त्री इस विषय को ले कर राजा के पास गया। राजा ने कहा कि वह अपने मन्त्रियों की भावना का सम्मान करता है; किन्तु मुख्यमन्त्री को चाहिए कि वह स्वयं अपने अनुभव से ही इसका उत्तर दे। राजा ने उसे भवन में निवास कर रहे पुण्यात्माओं के नामों की सूची दी और आदेश दिया कि मुख्यमन्त्री उन सबको तथा मन्त्री गण को उसके सदन में एक विशिष्ट भोजन का आमन्त्रण दे और उन सबको रात्रि-भर का अभ्यागत बनाये। मुख्यमन्त्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रातः की अल्प वेला में नृत्य और संगीत के मध्य भोजन-विशेष होता रहा। सभी पुण्यात्मा अवसर को सफल बनाने के लिए तथा प्रवचन देने के लिए विद्यमान थे। राजा ने मुख्यमन्त्री से कहा कि वह प्रातःकाल पाँच-छह बजे के लगभग कुछ सेवकों को अनिद्र करने के लिए प्रत्येक के ऊपर शीतल जल छिड़के। मुख्यमन्त्री के आदेश अनुसार कार्य किया और सबसे पहले पुण्यात्माओं को अशिष्ट रूप से जगाने के लिए सेवकों को साथ लिया। वे 'राम-राम-राम', 'ॐ ॐ ॐ' कहते हुए तत्काल जाग उठे। प्रत्येक साधु इसी प्रकार भगवन्नाम का उच्चारण करते हुए जागृत हुआ। मुख्यमन्त्री ने इसे विचार में रख कर मन्त्रियों के निवास-स्थानों तक अपने सेवकों का अनुगमन किया। यथा तथा, उनमें से प्रत्येक अभिशाप देते हुए, अपशब्द कहते हुए अत्यन्त क्रोध के साथ अनिद्र हुआ। इस दृश्यावलोकन हेतु राजा वहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा- "क्या अब आप देखते हैं कि पुण्यात्माओं और मन्त्रियों के हृदय में कितना अन्तर है? अब आप जान गये होंगे कि मैं पुण्यात्माओं का इतना सम्मान क्यों करता हूँ और उनकी संगति में रहने का प्रयास क्यों करता हूँ। उनके लिए तो सर्वत्र ब्रह्म ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। वे भगवद्-भाव से परिपूर्ण हैं और ये मन्त्री गण सब प्रकार की लौकिक योग्यता होते हुए भी-तुमने देखा ही है, इनके अन्तःकरण में क्या है! अतः सन्त भगवद्-भाव से पूर्ण हैं और इनके माध्यम से ही भगवान् स्वयं को प्रकट करते हैं।
१६.दिव्य जीवन
धन्य अमर साधको! शाश्वत दिव्य ज्योति की आनन्दमयी रश्मियो! मित्रो! महान् गुरु, गुरुदेव स्वामी शिवानन्द के नाम से आपका 'दिव्य जीवन' में अभिवादन करता हूँ।
आपमें से जो भक्त इस सभा में नये आये हैं अथवा प्रथम बार आज यहाँ समवेत हुए हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और विशेषतः प्रथम बार आये हुए व्यक्तियों को अपना स्नेह एवं सद्भावनाएँ प्रेषित करता हूँ।
इस 'दिव्य जीवन' की सभा में हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी सभा के द्वार सर्व समुदायों के लिए खुले हों। हमारा समुदाय ब्रह्मजिज्ञासुओं के सर्व समुदायों का आलिंगन करता है और बिना किसी भेद भाव के हम सब साधकों के साथ एक-रूप हैं। यह सर्वथा अगण्य है कि वे किसी धर्म-विशेष, मत अथवा चर्चा में निष्ठा रखते हैं या नहीं। अतः हिन्दू, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, पारसी तथा अन्य जनगण जिन्होंने अभी तक कोई धर्म ग्रहण नहीं किया है; किन्तु सुख-शान्ति की भद्रतर कला, आत्मोत्थान और अपनी प्रकृति की परिष्कृति की आकांक्षा करते हैं, ऐसे सभी साधकों का यहाँ स्वागत है। इसीलिए इस समुदाय को सर्वथा अनधिष्ठित अभिधान 'दिव्य जीवन संघ' दिया गया है। दिव्य स्वरूप परमात्मा के सभी जिज्ञासुओं का हम अभिवादन करते हैं। हम उन सबका स्वागत करते हैं जो दिव्य तत्त्व की खोज में जीवन यापन करते हैं और दिव्य रूप से जीने की इच्छा करते s/6 और इसी हेतु दिव्य जीवन के सौजन्य से पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ।
दिव्य जीवन क्या है?
दिव्य तत्त्व की जागृति में जीवन वास ही दिव्य जीवन है। अपने यथार्थ दिव्य प्रकृति के पूर्ण चैतन्य में तथा शरीर और मन से स्वयं को अतीत जान कर शाश्वत, सर्वशुद्ध और परिसम्पन्न आध्यात्मिक सत्ता के ज्ञान से युक्त जीवन व्यतीत करना ही दिव्य जीवन है। वही आपकी सत्ता का अन्तस्तम प्रधान सत्य है। वही आपकी वास्तविक प्रकृति का यथार्थ तथ्य है। आप दिव्य हैं। आप आध्यात्मिक हैं। अतएव आप अनश्वर और सर्वदा पूर्ण हैं। जिस प्रकार प्रत्येक सूर्य-रश्मि सूर्य की तेजस्वी एवं प्रकाशमयी प्रकृति का अंश है, उसी प्रकार आप शाश्वत सत्ता के अंश हैं और अपने अस्तित्व परमात्मा के अक्षय्य स्रोत हैं। जैसा स्रोत होगा, वैसा ही उद्गम होगा। अतएव परमात्मा दिव्य, सदा शुद्ध और अखण्ड होने के कारण उससे प्रसृत प्रत्येक वस्तु दिव्य, सदा शुद्ध और सदा अखण्ड होती है। उसकी प्रकृति अनिर्वचनीय, आनन्दमयी और परम शान्तिमयी होती है। अपनी वास्तविक प्रकृति में वास ही दिव्य जीवन में वास है। अपने सभी विचारों, भावों तथा अनुभावों, अपनी वाणी और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अपने कर्मों तथा व्यावहारिक जीवन के माध्यम से सदा दिव्य प्रकृति की अभिव्यक्ति हेतु निरन्तर जीना ही दिव्य जीवन है।
आज संसार को दिव्य जीवन की महती आवश्यकता है। सांसारिक व्यक्तियों को ही नहीं, प्रत्युत सर्व राष्ट्रों सम्प्रदायों, सर्व जन-समुदायों, धर्मों, देशों तथा आज संसार की उन्नति में यत्नरत सभी जनों को इसकी आवश्यकता है; क्योंकि मनुष्य में निहित उच्चतर प्रकृति की अभिव्यक्ति के प्रयास में ही इस युद्ध-पीड़ित, कष्ट के समय में इस महान् और अवसरवादी युग से, जो अद्भुत उपलब्धियों और विकास योजनाओं से युक्त होने के साथ ही अविश्वास, परस्पर विद्वेष, असन्तोष, घृणा और द्वन्द्वों से अभिभूत है, एक श्रेष्ठतर विश्व के उद्भव की आशा है। दिव्य जीवन वस्तुतः व्यष्टिरूपेण तथा समष्टिरूपेण इस विश्व-मतभेद-रूपी क्लिष्ट समस्या का महान् उत्तर है तथा आध्यात्मिक मूल्यों के सर्वथा लोप की समस्या का सहज सुझाव है।
दिव्य जीवन महान् गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द का एक सन्देश है। यह दिव्य जीवन, जीवन की एक महान् कला है जिसका सम्पूर्ण आधुनिक युग में प्रसारण करने के लिए वे अनवरत प्रयत्नशील रहे।
दिव्य जीवन, व्यवहार में दिव्यता का जीवन। दिव्य जीवन हमारे दिव्य कर्मों, वाणी और विचार से अभिव्यक्त हमारी दिव्य प्रकृति का जीवन है। यह मानो इस भौतिक संसार के धरातल पर मनुष्य रूप में देवता की अभिव्यक्ति है। आभ्यन्तर रूप से सर्वसम्पन्नता की ओर उद्गम तथा बाह्यतः सौन्दर्य, प्रेम, भद्रता, शान्ति, नम्रता, निःस्वार्थपरता और सेवाभाव के रूप में दिव्य जीवन यापन करना चाहिए; क्योंकि ये सब महान् गुण उस नित्य अखण्ड दिव्य प्रकृति के अभिन्न अंग हैं जो आपके भीतर विराजमान है और आपके प्रज्ञापूर्ण चेतन प्रयास द्वारा उन्मीलन तथा अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा में है।
दिव्य जीवन का मनुष्य महान् आदर्श के लिए जीवित रहने की आकांक्षा करता है। 'दिव्य जीवन' का सदस्य शान्ति का परिस्थापक है; क्योंकि वह सर्व मानवता की शाश्वत आध्यात्मिक एकता के दर्शन करता है। वह जानता है कि एक महान् सत्त्व सम्पूर्ण जीवन को एक अखण्ड सूत्र में बाँधता है, इसलिए वह सदा सम्पूर्ण विश्व का दिव्य सत्त्व की अभिव्यक्ति के रूप में अवलोकन करता है और सबसे आदर और प्रेम से व्यवहार करता है। वह मनुष्य में भगवान् के दर्शन करता है और इस प्रकार पूजा भाव से जीने की इच्छा करता है। वह इस अन्तरस्थ दिव्यता को प्रेम के रूप में पूजा अर्पित करता है।
इस दिव्य जीवन का अभ्यास करने वाला पुरुष प्रेम, परस्पर सम्मान तथा आदर का प्रसरण करता है। वह सद्भाव एवं बोध के लिए कर्म करता है और सदा महत्तर आध्यात्मिक समन्वयता लाने की इच्छा करता है। 'दिव्य जीवन' में आचरण करने वाला व्यक्ति जहाँ-कहीं भी जाये, जन-समूह को जीवन की एकता और भ्रातृभाव का आभास करायेगा। 'दिव्य जीवन' का अनुयायी सेवा और निःस्वार्थ भाव का महान् दृष्टान्त है। आभ्यन्तर आध्यात्मिक रूपान्तरण का यह बाह्य पक्ष है जो प्रत्येक व्यक्ति योग के द्वारा व्यावहारिक धर्म, प्रार्थना, आराधना भाव तथा सात्त्विक जीवन द्वारा लाने की आकांक्षा करता है।
मानव-जन्म का महत्त्व
संसार के प्रत्येक पदार्थ को प्रकाशित करने वाला वह परम तत्त्व आविर्भाव की अभिव्यक्ति से परे है अर्थात् अप्रकट रूप है। नाम-रूप की सृष्टि के अभाव में भी उसका अस्तित्व रहता है। विश्व नहीं रहता और ब्रह्माण्ड भी नहीं रहता। न तो स्थूल तत्त्व रहता है और न ही गति होती है। प्रत्युत रहती है एक अद्वितीय नितान्त, अक्षय्य निःशब्दता। तब किसी भी भौतिक वस्तु और गति का अभाव होने पर भी शुद्ध चैतन्य विद्यमान रहता है और तब शुद्ध चैतन्य परम इच्छा-शक्ति रूपी कर्म के द्वारा स्वयं को गतिशील बनाता है। इस गति से, भारतीय दर्शन के अनुसार, सूक्ष्म द्रव्य अथवा प्रकृति का अस्तित्व जागृत होता है। तब प्रकृति से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है। आत्मा अथवा परम तत्त्व से प्रकाश का उद्भव होता है। परमात्मा से इच्छा, परमात्मा से ही प्रेम और उसी से अन्तरिक्ष से ले कर जल पर्यन्त सभी तत्त्व उत्पन्न होते हैं। भौतिक प्रमाण के रूप में भौतिक जगत् को परमात्मा पोषण करता है। ऊपर असीम आकाश और चारों ओर असीम सागर आपको उस आत्यन्तिक परम तत्त्व का स्मरण कराते हैं। आत्यन्तिक परम तत्त्व से असंख्य ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति होती है। पुनरपि शुद्ध चैतन्य पूर्णतया अप्रभावित रहता है। सूर्य की किरणें गंगा के पवित्र जल, उदधि, झरनों, तालाबों, सरोवरों और पंक जलाशयों पर पड़ती हैं; किन्तु इस सम्पर्क से सूर्य कदापि प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से अन्य उद्भवों अर्थात् असंख्य ब्रह्माण्डों से भी परम तत्त्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्व और ब्रह्माण्ड पुनरपि, परमात्मा की इच्छा से शुद्ध चैतन्य द्वारा प्रचालित गति से सत्ताशील रहते हैं।
गति अथवा शक्ति शुद्ध चैतन्य से पृथक् नहीं है। यह मात्र शुद्ध चैतन्य का ही अभिव्यक्त साक्षात् स्वरूप है। अभिव्यक्ति स्थल, स्थूल तत्त्वों के अभाव में गति और शक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता। अतः सूक्ष्म तत्त्व अथवा प्रकृति की संरचना सर्वप्रथम हुई।
सूक्ष्म तत्त्व अथवा प्रकृति तीन गुणों द्वारा क्रियाशील हुई और इसने स्वयं को विविध स्थूलतर भागों में विभाजित किया। स्थूलतर भाव और अधिक स्थूल हो गये और विविध ब्रह्माण्ड बन गये। ब्रह्माण्डों से लोकों की संरचना हुई। लोकों में जीवन के विविध रूपों का उद्भव हुआ। अन्ततोगत्वा सार्वभौम गति अथवा चेतना मनुष्यों में अभिव्यक्त हुई जो लोकों में उद्भूत अन्तिम चिह्न थे। मानव में मन का सृजन किया गया। एवंविध मन दृश्य, विवेक और बोध की सर्वाधिक सशक्त शक्ति है।
प्रारम्भ में मानव-मन स्थूल था, केवल सहजावबोधयुक्त जो पशु की अपेक्षा थोड़ा अधिक निपुण था। किन्तु सृष्टि की उन्नति के साथ ही यह शनैः शनैः परिष्कृत होने लगा। मानव-मन ने जब उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर लिया, तब निम्नतर और उच्चतर मन की पृथक् जागृति उद्दीप्त हुई। निम्न मन स्थूल द्रव्यों के साथ एकरूप हो गया। इस प्रकार से ससीम चैतन्य तद्रूप हुआ; किन्तु उच्चतर मन सदा उस शाश्वत चैतन्य की खोज में रहा। यह मन सीमा, बन्धन और कारावास से असन्तुष्ट था। अतएव इसने जीव की वास्तविक प्रकृति की खोज में निरूपण प्रारम्भ किया। उसका बोध हो जाने पर मानव में सीमित चैतन्य से मुक्त होने पर, पुनः असीम सर्वसम्पन्न परम स्रोत में लीन होने पर चक्र समाप्त होता है। यह एक चक्र है। यह आपकी मानवीय प्रकृति मानव-जन्म का सच्चा अर्थ है। चक्र को पूर्ण करके आध्यात्मिक गरिमा की पराकाष्ठा को प्राप्त करो। 'दिव्य जीवन' यापन का अभिप्राय है-इस उपलब्धि के रहस्य का चेतन रूप से यहीं और अभी उद्घाटन करना।
आज का शुभ दिन मेरे सन्देश के श्रोताओं के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि आज २ अक्तूबर भारत में इस शताब्दी के महानतम पुरुष का जन्म-दिवस है जिसने उस सच्चे परमात्मा तक पहुँचने और उसका साक्षात्कार करने की आकांक्षा से पूर्ण दिव्य जीवन की प्रतिमूर्ति को अपने भीतर स्थापित किया। यह मानव थे- श्रद्धेय महात्मा गान्धी। आप सब भारत के राष्ट्रपिता से परिचित हैं जो भारतीय स्वतन्त्रता के निर्माता थे। उस साधु पुरुष ने अहिंसा, प्रेम द्वारा घृणा पर विजय प्राप्त करने की कला का सिद्धान्त और व्यवहार में उद्विकास किया। तीन सहस्र वर्ष पूर्व पूजााई बुद्ध के, वे बीसवीं शताब्दी के अवतार थे। महात्मा गान्धी दिव्य जीवन की सजीव प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने निज व्यक्तित्व में दिव्य जीवन को कैसे उतारा, इस विषय पर मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ और मेरे विचार में उनके जन्म-दिवस पर यह उन्हें अत्यन्त भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी ।
भारत में, महात्मा गान्धी की जन्म शताब्दी पर ठीक इसी समय कार्यक्रम चल रहे होंगे; क्योंकि अभी भी महात्मा जी की न केवल राजनीतिज्ञ के रूप में, प्रत्युत एक पूजार्ह साधु के रूप में आराधना की जाती है जिसने महान् भारतीय ऋषियों के सन्देश, धर्म-सन्देश का पुनरुत्थान किया। धर्म का अभिप्राय है-नीति, प्रार्थना, दृढ़ बाह्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा पर आधारित जीवन ! एवंविध महात्मा गान्धी महर्षियों के अर्वाचीन प्रतिनिधि थे जिन्होंने हमें सांस्कृतिक आदर्श प्रदान किया। उनके नाम पर मैं आपके समक्ष महान् गान्धीवादी जीवन-आदर्श को संक्षेप में रखने की आकांक्षा करता हूँ।
आध्यात्मिक जिज्ञासु के रूप में महात्मा गान्धी
अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में महात्मा गान्धी ने कहा- "जो लोग मुझे राजनीतिज्ञ समझते हैं और सोचते हैं कि मेरा व्यवसाय राजनीति है, वे वस्तुतः मुझे नहीं समझते, वे मेरे आभ्यन्तर व्यक्तित्व से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। मैं एक साधक हूँ अथवा किंचिदपि नहीं। मेरे जीवन का सत्य है मेरी जिज्ञासा, ईश्वर की खोज। राजनीति तो मेरे जीवन का एक आकस्मिक अंश है।" गान्धी सदा महान् सत्य की खोज में निरत रहे और यह जिज्ञासा उनमें बाल्यकाल में ही जागृत हुई। वह अत्यन्त धार्मिक और सात्त्विक माता-पिता के अत्यन्त भक्तिमत् पुत्र थे। अभी वह उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्र थे तभी से उन्हें राम-नाम का जप करने का अभ्यास हो गया। उनकी जिज्ञासा बढ़ती गयी और इसने कोटिशः भारतीय निर्धन जनता में साक्षात् परमात्मा की सेवा का स्वरूप धारण किया। उन दिनों भारत राजनीतिक दौर से गुजर रहा था। इसीलिए उनकी सेवा ने जनपद के कल्याण हेतु राजनैतिक उत्तेजना का रूप धारण कर लिया। महात्मा गान्धी के लिए यह सब उनकी भगवद्-आराधना का ही एक अभिन्न अंग था। मनुष्य में और मनुष्य के द्वारा, भारत के पीड़ित जनों में और उनके माध्यम से अपने निर्धन बन्धुओं में और उनके निमित्त से (भगवद्-पूजा), यह सब उनकी साधना थी। गान्धी जी का जीवन पूर्णतया सत्य, पवित्रता और दया के आदर्श पर आधारित था और सेवा का पथ ही उनका पथ था। उनके जीवन में हम आत्म-संयम, अनवरत आभ्यन्तर पिपासा, समन्वय और उत्कृष्ट सरलता के आदर्श का दर्शन करते हैं जिसका समानान्तर विश्व में किसी ने कदाचित् ईसा के जीवन के अतिरिक्त विरल ही कहीं देखा होगा। अनेक लोगों ने उन्हें अर्वाचीन ईसा कहा है। अन्य जनों ने उन्हें आधुनिक सेंट फ्रांसिस और आधुनिक बुद्ध की संज्ञा दी है। वे सम्पूर्ण आधुनिक विश्व के लिए प्रेरणा का महान् स्रोत रहे हैं और इस शताब्दी में आने वाले वर्षों में विश्व उनके सम्बन्ध में और अधिक श्रवण करेगा।
महात्मा गान्धी की महान् आध्यात्मिक शक्ति का केन्द्र उनकी शिक्षा नहीं थी; क्योंकि वे तो निर्धनता का जीवन यापन करते और उनके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत उनका ईश्वर के साथ अनवरत अटूट सम्पर्क था। उन्होंने ऐसा सम्पर्क कैसे स्थापित किया? दैनन्दिन प्रार्थना और दिव्य नाम द्वारा वे सन्ध्या की वेला में सर्व अन्य कृत्यों को त्याग कर, उनसे विमुख हो जाते। बिना इसके उनका एक भी दिवस व्यतीत न होता। सूर्यास्त होने पर गान्धी सदा अपने छोटे-से प्रार्थना-समूह में, कदाचित् एक विशाल बड़ के वृक्ष के नीचे किसी शान्त स्थान में, किसी प्रांगण के एक कोने में एक लकड़ी के बने उच्च स्थान पर, शेष संसार से पूर्णतया विरक्त, ब्रह्म के साथ आभ्यन्तर संयोग की एक अद्भुत शान्ति और माधुर्य में लीन देखे जाते।
उनकी प्रार्थना-सभाएँ असामान्य थीं। ईश्वर तक उनकी पहुँच की दृष्टि की सार्वभौमिकता एक प्रकार से सबके लिए एक अनुकरणीय पाठ थी। उनकी प्रार्थना में अरबी भाषा में गायी जाने वाली कुरान के अंश, पारसी भाषा में उच्चारित पारसी के जेन्दावस्ता के अंश, जापानी भाषा में कहे जाने वाली जापानी प्रार्थना के अंश, वेदों के संस्कृत में स्तोत्र, टेस्टामैंट के अंश और भगवान् कृष्ण की प्रार्थना के अंश होते। एवंविध, प्रायः सभी धर्मों का महात्मा गान्धी की सायं प्रार्थना में प्रतिनिधित्व होता।
मौन की वेला होती जिसमें सब ध्यानमग्न हो जाते। सामूहिक दिव्य नाम-जप होता तथा तदुपरान्त मौन, ध्यान और सम्भाषण से बाहर आ कर महात्मा गान्धी जनपद को पाँच-दस मिनट का एक अल्प सन्देश-प्रसारण करते जो सदा आध्यात्मिकता से पूर्ण तथा सजीव होता और जो उनकी दैनन्दिन प्रार्थना में परमात्मा के साथ तत्काल सम्पर्क से प्राप्त होता।
मूलतः गान्धी प्रार्थना-पुरुष थे। निष्ठा और दैनिक प्रार्थना में उनका मूल था। वे कहते-"प्रार्थना ही मेरे जीवन का वास्तविक भोजन है। बिना प्रार्थना के मेरा जीवित रहना असम्भव है।" उनके संघर्षपूर्ण जीवन की सर्व महान् उपलब्धियों का रहस्य था दिव्य नाम! दिव्य नाम गान्धी की अनवरत शक्ति और आश्रय था। वे दिव्य नाम राम-नाम से कभी विलग नहीं हुए। हिन्दू होने के कारण उनके लिए यह 'राम' नाम था; किन्तु मूलतः यह दिव्य नाम ही था जो सदा उनके अधरों पर रहता और सदा उनके जीवन की अनवरत शक्ति था जिसके प्रति कुछ लोग तो संशय करते और अन्य कुछ को विदित था और जानने वालों में बहुत कम ही इसके सच्चे महत्त्व से अवगत थे।
महात्मा गान्धी के सब कार्य संसार से नितान्त विरक्ति और प्रेम द्वारा भगवान् में गहन आभ्यन्तर आसक्ति, आराधना-भाव, प्रार्थना और आध्यात्मिक योग में अनवरत दिव्य नाम-जप से युक्त परमात्मा में केन्द्रित होते। समस्त जीवन पर्यन्त महात्मा गान्धी के लिए भगवान् ही सर्वस्व थे। राजनैतिक उपलब्धि भी नहीं, किन्तु केवल भगवान् का ही उनके जीवन में आत्यन्तिक मूल्य था। वही केन्द्र था, वही लक्ष्य था, उनकी खोज का विषय इतने सुन्दर ढंग से व्यतीत किये गये उनके सम्पूर्ण जीवन का उद्देश्य वही परब्रह्म था। यह दिव्य जीवन महात्मा गान्धी की सतत खोज थी। वे कर्म द्वारा स्वजनों की सेवा तथा दिव्य तत्त्व की सेवा करते जिसकी अनुभूति उन्होंने सर्व हृदयों में विराजमान परमात्मा के रूप में की।
स्वकर्मों का आध्यात्मीकरण करो
अतएव स्वकर्मों को आध्यात्मिक बनाओ। दिव्य जीवन व्यतीत करने के लिए अपने सभी अध्ययन, वचन, क्रीड़ा आदि को प्रभु के अर्पण कर दो। अनुभव करो कि सम्पूर्ण जगत् में वही व्याप्त है। आपकी सन्तान भगवान् की ही अभिव्यक्ति है, ऐसा अनुभव करो। ऐसे आभ्यन्तर आध्यात्मिक भाव से मानवता की सेवा करो। तब आपकी सभी दैनिक क्रियाएँ आध्यात्मिक अभ्यास में रूपान्तरित हो जायेंगी। वे योग में परिणत हो जायेंगी।
प्रत्यार्ह अपने नित्य कर्मों के साथ-साथ ही आपको यह आन्तरिक सम्पर्क, दिव्य स्रोत के साथ प्रार्थना, आराधना और एकान्त ध्यान द्वारा योग स्थापित किये रखना है। यह आपका प्रथम कर्तव्य है। किसी भी कारण से इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रातः ब्राह्ममुहूर्त में जागो और ध्यान का अभ्यास करो। कतिपय योग-मुद्राओं का अभ्यास करो-शरीर की उपेक्षा मत करो। थोड़ा प्राणायाम भी करो। धर्मग्रन्थों का अध्ययन करो। यह आभ्यन्तर मौन और ध्यान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। आध्यात्मिक अभ्यास हेतु प्रभातकाल उतना ही महत्त्वपूर्ण है। प्रातः एवं सायं, धूलिवेला में कुछ समय के लिए भी ध्यानाभ्यास अतीव महत्त्वपूर्ण है।
विचार की पृष्ठभूमि (मानसिक जप), भगवद्-चिन्तन का अभ्यास करो। सावधान-इसकी उपेक्षा नहीं करना। अपने दिव्य आदर्श का चिन्तन स्वरूप बनो। प्रत्येक व्यक्ति की किसी-न-किसी विचार की पृष्ठभूमि होती है; किन्तु प्रायः यह लौकिक, जघन्य (कुत्सित) अथवा भौतिक होती है। एक वकील की मानसिक विचारधारा श्रावक, न्याय-सभा अथवा न्याय के नियमों आदि से पूर्ण होगी। एक चिकित्सक के विचारों की पृष्ठभूमि अस्पताल, इन्जैक्शन, रोगी, औषधि, शुल्क आदि से परिपूर्ण होगी। दादी माँ अपने पौत्र एवं पुत्रों का ध्यान करेगी। दिव्य जीवन के अभ्यासी के विचारों की पृष्ठभूमि दिव्य प्राप्ति के गरिमामय आदर्श भगवान्, भद्रतापूर्ण जीवन और दिव्य नाम से युक्त होनी चाहिए। दिव्य गुणों का आरोपण करो। निषेधात्मक गुणों का निराकरण करो। विश्व के प्रति, सबके प्रति अपने मानसिक भावों को परिवर्तित करो। अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी व्यर्थ न गँवाओ। भद्र जीवन, प्रभु, दिव्य चिन्तन के आदर्श का चिन्तन और कीर्तन करो। भगवान् के लिए जीवन यापन करो। अपने नित्य कर्मों के समय प्रत्येक व्यक्ति तक जिसे भी आप मिलें, दिव्य सन्देश का प्रसारण करो। किसी मित्र को मिलने पर इधर-उधर की व्यर्थ की बातें करने की अपेक्षा उससे प्रश्न करो कि इन दिनों वह ध्यान की कौन-सी विधि का अभ्यास कर रहा है अथवा कौन-से नवीनतम आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन कर रहा है। यही आपका वार्तालाप होना चाहिए। आपके सम्बन्ध में प्रत्येक वस्तु भद्र और दिव्य हो, उत्कृष्ट हो। वृथालाप त्याग दो। उपन्यास पढ़ना छोड़ दो। वृथालाप और उपन्यास आपको मानसिक शान्ति प्रदान नहीं करेंगे। वे आपके मानसिक सन्तुलन को बिगाड़ते हैं। आपके मस्तिष्क को अनावश्यक, दुःखद, लौकिक विचारों से भर देते हैं। इनकी अपेक्षा अपने मस्तिष्क को उच्छ्रित दिव्य विचारों से परिपूर्ण करो। आपकी अन्तरात्मा दिव्य तेज से उद्दीप्त हो उठे। इस पर पवित्रता व्याप्त हो जाये।
सर्वदा स्मरण रखो कि यह संसार दुःख, पीड़ा, जरा और मृत्युमय है और आपका सर्वप्रथम कर्तव्य चक्र को पूर्ण करना भगवद्-साक्षात्कार करना, आत्मानुभूति करना है। केवल इसी में आप परम शान्ति, शाश्वत आनन्द, नित्य ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। कमर कसो। स्वयं को इस दिव्य जीवन में ढालने के लिए उद्यत हो जाओ। व्यावहारिक जिज्ञासु बनो। आप अमरत्व प्राप्त करेंगे। आप परम शान्ति एवं नित्यानन्द का उपभोग करेंगे, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं।
आपके सर्व कृत्यों में, उज्ज्वल भविष्य में, सर्वसम्पन्नता और परम दिव्यानन्द तथा परम पद में भगवान् आप पर आरोग्यता, दीर्घायु, शान्ति, समृद्धि, परम दिव्य आनन्द एवं परम पद की वृष्टि करें!
संक्षेप में दिव्य जीवन के मूल तत्त्व
अब मैं एक अल्प गीत के साथ उपसंहार करूँगा जिसमें गुरुदेव ने दिव्य जीवन, दिव्य वास और उन सद्गुणों का समावेश किया है जिन्हें मनुष्य को दिव्य जीवन के स्तम्भ स्वरूप स्वयं में अंकुरित करना चाहिए।
दिव्य जीवन के मूल तत्त्व हैं- पवित्रता, निःस्वार्थता, सेवाभाव, प्रेम (मानव- प्रेम और ईश्वर-प्रेम), नियमित ध्यान, आभ्यन्तर जीवन और अन्ततः परमात्मा का साक्षात्कार। अतएव दिव्य जीवन के सम्बन्ध में गुरुदेव गाते हैं :
सेवा, प्रेम, दान, पवित्रता, ध्यान, साक्षात्कार ।
भले बनो, भला करो, दयालु बनो।
खोजो, 'मैं कौन हूँ', आत्मज्ञान करो और मोक्ष पाओ ।।
सेवा, प्रेम, दान, पवित्रता, ध्यान, साक्षात्कार ।
भले बनो, भला करो, दयालु बनो।
संक्षेप में यह आपके लिए दिव्य जीवन है। इसी में आवागमन के चक्र, इस सांसारिक बन्धन से मुक्ति का उपचार, अद्भुत सर्व रोग-हर औषधि और सर्व चिकित्सा है। किन्तु जब आप औषध ग्रहण करते हैं, तो आहार के सम्बन्ध में आपको कतिपय नियमों का भी पालन करना होता है और ये हैं आहार के अष्टादश नियम :
प्रसन्नता, नियतता, निरभिमानता,
विमलता, सरलता, सत्यवादिता,
समचित्तता, स्थिरता, शालीनता,
युक्तता, नम्रता व संलग्नता,
(अखण्डता) पूर्णता, आर्यता, उदारात्मता,
दयालुता, उदारता, पुण्यशीलता ।।
इन सबका अभ्यास जो नित्य करता,
अचिरेण ही प्राप्त करता अमरता ।।
ब्रह्म ही है केवल नित्य सत्ता,
अमुक नाम स्वरूप तो है मिथ्या सत्ता।
धाम होगा आपका आत्यन्तिक नित्यता,
देखोगे आप भिन्नता में स्वयं एकता;
विद्यालय में इस ज्ञान की है दुर्लभता, '
आरण्य संस्थान' में ही है सुलभता ।।
इन दिव्य गुणों का नित्य अभ्यास करो। वे आपके जीवन को दिव्य बनाने में सहायक होंगे। वे आपके आभ्यन्तर आध्यात्मिक जीवन का आधार होंगे; क्योंकि बिना गुणों के आपका जीवन शुष्क है, गुणों के बिना आपका जीवन निरर्थक है और आपकी दिव्य प्रकृति को क्रीड़ा हेतु उपयुक्त क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता। दृढ़ संकल्प तथा ईश्वर और उसकी शक्ति में सहायतार्थ पूर्ण निष्ठा द्वारा जीवन को सर्व निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व को सर्वगुणों का कीड़ा-स्थल बनाने पर ही आप नित्यात्मा में दिव्य ज्योति के प्रकाश और (आपके द्वारा) इसके प्रसरण की पूर्ण आशा कर सकते हैं। ऐसा दिव्य जीवन वास करो। स्वयं को इन गुणों की प्रतिमूर्ति बनाओ। अपनी निम्न प्रकृति को पूर्णतया संयत करके स्वयं को अन्तरात्मा में केन्द्रित दिव्यता के तेजपुंज के प्रवाह हेतु स्रोत और साधन-रूप बनाओ। ऐसा है दिव्य जीवन !
ईश्वर करे, आप दिव्य हों! दिव्यता आपको प्रेरित करे और आपके सर्वकर्मों में आपका पथ-प्रदर्शन करे! आपका समस्त जीवन दिव्य जीवन का अलौकिक और उज्ज्वल दृष्टान्त हो! यही आपसे मेरी विनती है। यही आपसे आकंक्षा है। मेरे प्रिय मित्रो, दिव्यतापूर्ण हो कर जीवन यापन करो। निज दिव्य प्रकृति को विस्मृत करके चिन्ता के भ्रम-जाल में स्वयं को निक्षिप्त करके नहीं जिओ। अपनी दिव्य प्रकृति को प्रतिपादित करो और परमात्मा के उपवन में विस्मय-विमुग्ध करने वाले पुष्प, दिव्य सौन्दर्य को बिखेरते हुए सुन्दर, मनोहर कुसुम, दिव्य सुरभि, आध्यात्मिक सुरभि बनो! .
भगवान् आप सबको आशीर्वाद दें! आपकी अन्तरात्मा आपको प्रेरित करे! गुरुदेव शिवानन्द आप पर अपने आशीष की वृष्टि करें ! भूत और वर्तमान के पूर्वी और पाश्चात्य सन्त आपको आश्रय प्रदान करें और आपको दिव्य गौरवमयी प्रकृति के साक्षात्कार की ओर अग्रसर करें!
मेरे प्रिय साधको, आपके मध्य रह कर आप सबमें अदृश्य रूप से व्यष्टि रूप से विद्यमान परमात्मा को इन शब्दों द्वारा पूजा अर्पित करने का आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं पुनः आपका आभारी हूँ। सदा संगठित रहो। संगठित रह कर संगठित रूप से विचार करो, संगठित हो कर साधना करो, संगठन में कर्म करो और संगठित हो कर कर्मक्षेत्र में कूच करो। अनुभव करो कि आप एक हैं और इस एकता और मित्र भाव द्वारा आपके सम्पर्क में आने वाले सभी जनों को अनिर्वचनीय आशीष प्राप्त हों !
प्रभु करे, आप दिव्यता के महान् केन्द्र बनें! असंख्य जनों के लिए आध्यात्मिक जागृति के महान् केन्द्र बनें! प्रीति, समन्वय, एकता के केन्द्र एवं भातृ भाव तथा ऐक्य भाव के ज्वलन्त दृष्टान्त बनें! आने वाले वर्षों में आप दिव्य जीवन के आनन्द को समस्त विश्व में सम्प्रसारित करें!
ॐ
ॐ श्री गणेशाय नमः
ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय
इस पुस्तक की अनुवादिका श्रीमती गुलशन सचदेव (अलीगढ़) ने सन् १९६८ में दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.ए. (संस्कृत) की उपाधि प्राप्त की। गुरुदेव की अहेतुकी कृपा से कुछ पुस्तकों का अँगरेजी से हिन्दी माध्यम से अनुवाद करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इनके द्वारा अनुवादित कुछ पुस्तकों का उल्लेख इस प्रकार है- 'मुक्ति-पथ' : लेखक श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज, 'अध्यात्म की आधारशिलाएँ" : लेखक श्री स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज, 'श्रीमद्भगवद्गीता' : लेखक सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज इत्यादि । श्री स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज द्वारा की गयी माण्डूक्योपनिषद् की व्याख्या का हिन्दी रूपान्तर आजकल 'दिव्य जीवन' (हिन्दी मासिक पत्रिका) में प्रकाशित हो रहा है।
हरि ॐ तत्सत्!