वाराणसी: पुनर्खोज
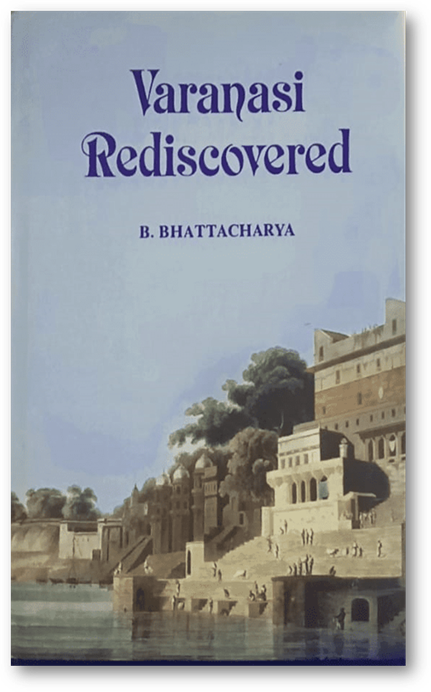
अनुवादक: रमेश चौहान
Varanasi
Rediscovered
B. Bhattacharya
वाराणसी: पुनर्खोज
अनुवादक: रमेश चौहान
With 40 black & white illustrations and 12 maps
Munshiram Manoharlal
Publishers
To the People of Varanasi
विषय-सूची
मानचित्र. 1. काशी दर्पण: पारंपरिक मानचित्र जिसे आज भी श्रद्धालु खोजते हैं ।
मानचित्र 2. वाराणसी के पर्यटकों के रेखाचित्र: अमेरिकी, फ्रांसीसी, जापानी और ग्रीक
मानचित्र 3: वाराणसी मंदिरों को दर्शाता शहर
मानचित्र 4. विश्वनाथ, मणिकर्णिका, दशाश्वमेध और आसपास
मानचित्र5: राजघाट पठार के साथ बनारस, जिसमें शुरुआती जल निकासी दिखाई गई है ।
मानचित्र 6. जेम्स प्रिंसेप का बुनारस का मानचित्र, जिसमें काशी के तालाब और झीलें दिखाई गई हैं
मानचित्र 7. ज्ञानवापी और मंदिर
मानचित्र 8: चौक क्षेत्र-पुराने और नए मंदिर
मानचित्र 9. क्रमिक परिवर्तन के साथ वाराणसी
मानचित्र 10. शहर का विकास: बनारस 1822
मानचित्र 11. वाराणसी: एक समग्र संज्ञानात्मक मानचित्र-रेखाचित्र
2. वाराणसी के नामों का शास्त्रीय संदर्भ
मानचित्र
1. काशीदर्पण: पारंपरिक मानचित्र, जिसे आज भी श्रद्धालु तीर्थयात्री खोजते हैं
2. वाराणसी के पर्यटकों के रेखाचित्र: अमेरिकी, फ्रांसीसी, जापानी और ग्रीक
3. वाराणसी: शहर, मंदिर दिखाते हुए
4. विश्वनाथ, मणिकर्णिका, दशाश्वमेध और आसपास
5. राजघाट पठार के साथ बनारस, जिसमें शुरुआती जल निकासी दिखाई गई है
6. जेम्स प्रिंसेप का बनारस का मानचित्र, जिसमें काशी के तालाब और झीलें दिखाई गई हैं
7. ज्ञानवापी और मंदिर
8. चौक क्षेत्र-पुराने और नए मंदिर
9. क्रमिक परिवर्तन के साथ वाराणसी
10. शहर का विकास: बनारस 1822
11. वाराणसी: एक समग्र संज्ञानात्मक मानचित्र-रेखाचित्र
12. अंग्रेजों द्वारा सड़क और रेलमार्ग निर्माण द्वारा इसे बाधित करने के बाद वाराणसी के विस्तारित शहर का एक मूल्यवान पुराना मानचित्र
रेखांकन
1. इस्लामी शासन के अंत में एक अज्ञात सैनिक द्वारा पूर्वी तट से देखी गई वाराणसी, विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, कलकत्ता में मूल पेंटिंग
2. चौकी घाट या नागा घाट से वाराणसी में गंगा का दृश्य
3. पुराने विश्वनाथ मंदिर का खंडहर, ज्ञानवापी में मस्जिद का पिछला भाग
4. कृतिवासेश्वर मंदिर, आज की तरह
5. खंडहर हो चुके सिंधिया घाट के साथ दत्तात्रेय और यम घाट
6. हरिश्चंद्र अंत्येष्टि घाट: उन्नीसवीं सदी के अंत में
7. बकरियाकुंडा (बरकारीकुंडा): उन्नीसवीं सदी के अंत में ली गई तस्वीर। लेखक ने 1929 तक इसे देखा और इसे बदतर पाया। अब कलाकृतियों का कोई निशान नहीं है
8. ओंकारेश्वर लिंगम
9. रानी भवानी की महिमा का स्मारक: दुर्गा मंदिर
10. रानी भवानी की महिमा का स्मारक: दुर्गाकुंड
11. मानमंदिर घाट: जेम्स प्रिंसेप द्वारा पेंटिंग
12. मानमंदिर का प्रसिद्ध झरोखा, विवरण, जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई पेंटिंग
13. नेपाली खपरा घाट, वाराणसी
14. शांत गंगा बहती है
15. राजघाट किला टीला-जहाँ खुदाई हुई थी
16. मणिकर्णिका घाट
17. मणिकर्णिका, चक्रतीर्थ और ब्राह्मणाला
18. ललिता घाट
19. ओंकारेश्वर मंदिर
20. मध्यमेश्वर मंदिर जिसके पीछे मृत्युंजय मंदिर है
21. कपिलधारा, जैसा कि जेम्स प्रिंसेप ने देखा
22. कृतिवासेश्वर आज: आलमगिरी मस्जिद का आंतरिक भाग, दिखा रहा है 'स्टंप' जहां माना जाता है कि गर्भगृह था, और अब शिवरात्रि के दिन इसकी पूजा की जाती है
23. पहाड़ी पर आदि विश्वनाथ
24. जेम्स प्रिंसेप द्वारा देखे गए विश्वनाथ मंदिर के खंडहर।
तीन कब्रों पर ध्यान दें
25. महान मंदाकिनीतालाव: जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाया गया। बड़ा गणेश माना जाता है कि यह दाहिने हाथ के ग्रोव के पीछे है
26. ज्ञानवापी का हमेशा चौकन्ना रहने वाला बैल नंदी
27. जेम्स प्रिंसेप द्वारा देखा गया बालाजी घाट
28. जेम्स प्रिंसेप द्वारा देखा गया भीम घाट
29. दशाश्वमेध घाट
30. तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते हैं (उन्नीसवीं सदी के मध्य में)।
31. चेत सिंह (किरकी घाट) में बुढ़वा मंगला मेला।
32. सिख महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सोने से ढंके विश्वनाथ मंदिर के टॉवर
33. काशी विश्वनाथ
34. पक्की-महल, चौखंबा, उन्नीसवीं सदी के मध्य: जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई पेंटिंग
35. लाट भैरों
36. गंगा पर मालवीय पुल, अग्रभूमि में मीर रुस्तम अली की कब्र के साथ
37. कपालमोचन तालाब की समाप्ति की अवस्था
38. बेनीमाधब में औरंगजेब की मस्जिद, अग्रभूमि में बालाजी का महल, जैसा कि जेम्स प्रिंसेप ने देखा
39. औरंगजेब की मीनारों से देखा गया आधुनिक वाराणसी शहर।
40. जेम्स
प्रिंसेप द्वारा देखा गया वाराणा में भरतमिलाप मेला
भूमिका
भारत में कोई और ऐसा शहर नहीं है जो विचारशील पर्यटकों में वाराणसी जितनी उत्सुकता जगाता हो। यह रुचि केवल आधुनिक नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास की नसों में प्राचीन काल से बह रही है। इतिहास के ज्ञात समय से, और भारत में यात्रियों के इतिहास में, हम पाते हैं कि चीन से लेकर ब्रिटिश द्वीपों तक, अफ्रीका से लेकर रूसी-जर्मन क्षेत्रों तक, और यहाँ तक कि विद्वान अरबी क्षेत्रों से भी व्यापारी, विद्वान, दार्शनिक और घुमक्कड़ जन वाराणसी के प्रसिद्ध शहर की ओर खिंचे चले आते थे।
यह प्रवृत्ति आज भी थमी नहीं है, बल्कि बढ़ रही है। एक के बाद एक किताबें इस अमर शहर, भव्य, रहस्यमयी, आकर्षक वाराणसी पर प्रकाशित हो रही हैं — एक ऐसा प्राचीन नगर जो कभी अपनी युवावस्था नहीं खोता।
जिन्हें इस जादुई शहर की धड़कनों को ‘महसूस’ करने का सौभाग्य मिला है, वे अक्सर अपनी पहली मुलाकात की प्रतिक्रियाओं को लिखने की प्रबल इच्छा से प्रेरित हुए हैं — एक ऐसा शहर जो ज्ञान, साहस और स्पष्टवादिता का प्रतीक है।
वाराणसी पर विदेशी लेखकों की सबसे पुरानी पुस्तकें चीनी और अरब यात्रियों की हैं। इसके बाद अफ्रीकी, फ्रांसीसी, जर्मन और अंग्रेज यात्रियों, अधिकारियों और विद्वानों की रचनाएँ सामने आईं। इस शहर के साहित्य में फोटोग्राफर, चित्रकार, कलाकार भी शामिल हैं, जिन्हें इस प्राचीन नगर को कैद करने, चित्रित करने, गाने या व्यंग्य करने से खुद को रोक पाना असंभव लगा।
वाराणसी पर लिखी गई पुस्तकों की सूची पृष्ठ दर पृष्ठ भर सकती है। हाल की एक व्यापक पुस्तक, "Varanasi, the City of Light" (वाराणसी: प्रकाश का नगर) डायना एल. एक द्वारा लिखित है, जिसने वाराणसी को उन विदेशियों से परिचित कराया जो पर्यटक के दृष्टिकोण से शहर की जानकारी चाहते थे। हालांकि, उन्होंने अपनी सीमाओं के भीतर एक सराहनीय कार्य किया, लेकिन एक गैर-हिंदू और विशेष रूप से एक श्वेत महिला होने के कारण, वे उन छुपे हुए स्थानों तक नहीं पहुँच सकीं, जिन तक केवल एक दृढ़ हिंदू की ही पहुँच हो सकती थी।
वाराणसी पर सबसे रसपूर्ण रचनाओं में से एक है डॉ. मोतीचंद द्वारा लिखित "काशी का इतिहास"। यदि उन्हें स्वतंत्रता के बाद लिखने का अवसर मिला होता, तो वे निश्चित रूप से विषय पर और विस्तार से लिख सकते थे। ब्रिटिश राज के दौरान लेखन आसान नहीं था, विशेष रूप से एक सामाजिक आलोचक के लिए। और इतिहास क्या है, यदि वह अपने समय की आलोचना न करे? उनका कार्य, जितना भी प्रशंसनीय और विस्तृत है, वह अधिक तीव्र और खोजपरक हो सकता था। परंतु 1947 से पहले एक भारतीय के लिए सामाजिक आलोचना का रुख अपनाना अत्यंत कठिन था। और इतिहास बिना आलोचनात्मक दृष्टिकोण के इतिहास नहीं होता।
एक दुर्लभ रत्न है — मन्मथ नाथ चक्रवर्ती की बंगाली पुस्तक "काशीधाम"। लगभग आठ दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक कभी-कभी हिंदुत्व की अतिशयोक्ति में डूब जाती है, गैर-हिंदू समुदायों की आलोचना करती है, और अंग्रेजों की प्रशासनिक दक्षता की अत्यधिक सराहना करती है। फिर भी, इसमें दी गई जानकारियों की मात्रा, गुणवत्ता और व्यवस्था सराहनीय है, बशर्ते कि कुछ अशुद्धियों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए।
विश्वनाथ मुखर्जी की "काशी" और एल. पी. विद्यार्थी की "The Sacred Complex of Kashi", साथ ही के. एन. शुक्ला की "Varanasi: Down the Ages", आलोचनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और निश्चित रूप से ई. बी. हैवेल और एम. ए. शेरिंग के कार्य आज भी शास्त्रीय माने जाते हैं।
फिर भी, यह प्रयास एक बहाना पेश कर सकता है। यह निश्चित रूप से पहले किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति से बचने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक पुरातात्विक दृष्टि से पूरी तरह मौलिक कार्य नहीं है। लेखक ने उन क्षेत्रों को छूने का प्रयास किया है, जिन्हें शायद अत्यधिक विवादास्पद मानकर कभी छुआ ही नहीं गया।
इस पुस्तक ने वाराणसी के अतीत के ‘क्या’, ‘क्यों’ और ‘कैसे’ की गहराई में जाने का प्रयास किया है। वाराणसी की विशिष्ट सामाजिक मान्यताएँ, स्वरूप, जटिलताएँ, जनसंख्या-वितरण, विशेष रूप से इसकी बहु-आयामी मानव समस्याएँ और उपलब्धियाँ, जो अवध और बनारस के राजा बलवंत सिंह की प्रभावशाली संस्कृतियों के साये में पनपीं, ने लेखक का ध्यान मंदिरों, मोहल्लों और घाटों की मात्र सूची से कहीं अधिक आकर्षित किया है।
यह पुस्तक वाराणसी को हड़प्पा युग से लेकर वर्तमान तक देखने का प्रयास करती है, पुराणों में दी गई बहुमूल्य जानकारी, इलाकों के नाम, भूले-बिसरे प्राकृतिक स्थलों के माध्यम से शहर की वास्तविक प्राचीन स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की कोशिश करती है।
कई वाराणसीयाँ रही हैं; आज जो शहर खड़ा है, वह कभी के वास्तविक स्थान से भिन्न है, जिसे अब कोई याद भी नहीं करता। शहर आज भी अपने कई नामों को दोहराता है, बिना यह समझे कि वे नाम क्या दर्शाते हैं और उनके भीतर कौन से ऐतिहासिक संकेत छिपे हैं, जो एक नए, अद्भुत वाराणसी को उजागर कर सकते हैं, जैसा कि पहले किसी भी लेखक ने कल्पना नहीं की थी।
यह पुस्तक स्थानीय क्षेत्रों के नामों को गंभीरता से लेती है, खोई हुई नदियों और झीलों को पुनः खोजने का प्रयास करती है, और गिरवाण पदमंजरी, कृत्य कल्पतरु, तीर्थ विवेचनाकाण्ड, काशी महात्म्य, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, और विशेष रूप से स्कंद पुराण के काशी खंड जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के माध्यम से वाराणसी के वास्तविक प्राचीन स्वरूप को सही परिप्रेक्ष्य में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है।
इस पुस्तक की टंकण प्रक्रिया में श्री शंकरसन बाणिक की सहायता प्राप्त हुई है, और लेखक श्री बिकाश बिस्वास के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हर कदम पर सहयोग दिया।
'टिप्पणियाँ' पाठ के अंत में दी गई हैं, जो कुछ विवादास्पद और अस्पष्ट बिंदुओं को स्पष्ट करने और पाठकों का ध्यान मौलिक स्रोतों की ओर आकर्षित करने के लिए हैं।
नई
दिल्ली बी.
भट्टाचार्य
फाल्गुनी पूर्णिमा, 1998
मानचित्र

मानचित्र. 1. काशी
दर्पण: पारंपरिक मानचित्र जिसे आज भी श्रद्धालु खोजते हैं
।
1. सनातन निवास
I
कौन नहीं जानता वाराणसी को? या, कौन जानता है?
वेन्स, काहिरा, बगदाद, दमिश्क, पेइचिंग, रोम — ये वो नाम हैं जो महाकाव्यों, कथाओं और दंतकथाओं में ‘प्राचीन’ के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन
वाराणसी के सामने ये सब आधुनिक लगते हैं। ये शहर जीवित हैं, आज
भी हलचल से भरे हुए हैं।
हम उन शहरों की बात नहीं कर रहे जो इतिहास के पन्नों में दब चुके हैं:
थेब्स, उर, नॉस्सस, ट्रॉय, पर्सेपोलिस, बोगोज-कोई, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। हम मरी हुई संस्कृतियों की बात नहीं कर रहे।
वाराणसी एक दूर की प्रतिध्वनि है, जो सदियों से चली आ रही है। वह आज भी जीवंत है, धड़क रही है, गूँज रही है। हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो आज भी जीवित है। जब हम वाराणसी की बात करते हैं, तो हम एक कार्यशील नगर की बात करते हैं।
जब आर्य जातियाँ अपने घोड़ों के साथ रेगिस्तानी इलाकों और पहाड़ी दर्रों को पार कर रही थीं, तब वे हरे-भरे खेतों और सुरक्षित आश्रयों की तलाश में कोकेशस, एलबुर्ज़, हिंदुकुश और बदख्शान की कठिन पहाड़ियों को पार कर रहे थे। वे दाश्त-ए-लूत, सरहद, बलूचिस्तान और आखिरकार थार के रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़े। वे ऐसे आए जैसे भेड़िए भेड़ों के झुंड पर टूट पड़ते हैं।
वह सचमुच बहुत पुराना समय था। सरस्वती नदी तब भी हिमालय से लेकर कच्छ और समुद्र तक अपनी निर्मल धारा बहा रही थी, पवित्र पुष्करावती गाँव से गुजरती हुई।
जब ये भूखे योद्धा ‘दूध और शहद की भूमि’ पर पहुँचे, तो उन्होंने अपने घोड़े और मांसाहार के दिन भुला दिए। वे खेती करने लगे और बसने लगे। उन्होंने इंद्र, पर्जन्य, वसुंधरा (बादल, गर्जना, बारिश और उपजाऊ धरती) के गीत गाए।
ये सवार एक अलग जीवन शैली के लोग थे। उनका अचानक आना उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका था, जो इस धरती के आदि निवासी थे — वे लोग जो इस धरती के प्राचीन निर्माता थे, जिन्होंने अपने गाँव और नगर खुद बसाए थे। उनका अतीत इतना प्राचीन था कि वह इतिहास की सीमाओं से भी परे था।
और वाराणसी ने उन आक्रमणकारी भीड़ का सामना किया। वाराणसी आर्यों से भी पुरानी थी।
आज हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि वे मूल निवासी कैसे रहते थे — आधा ग्रामीण, आधा शहरी, थोड़े परिष्कृत, थोड़े घुमंतू।
उन पाषाण युगीन लोगों के देवता आकाश में और उससे परे निवास करते थे। उनकी कृपा बारिश के रूप में बरसती थी, और उपजाऊपन का वरदान देती थी।
उनके देवता मुख्य रूप से प्रजनन की रहस्यमयी शक्तियों से जुड़े थे। आकाशीय शक्तियाँ सबसे अधिक मानव गर्भ के माध्यम से प्रकट होती थीं। जन्म और जीवन की इस पीड़ा-सुख, सुख-पीड़ा की गुत्थी ने उन्हें विस्मित कर दिया था, और वे जीवन के रहस्य की पूजा करते थे।
लेकिन इस शांत, चरवाहों जैसे जीवन पर एक महाविनाशकारी आपदा आ गिरी।
दूर-दूर से हजारों नंगे खुरों की आवाज आखिरकार थम गई। भूखे सवारों ने एक शांतिपूर्ण समाज पाया, जो धरती को उपजाऊ बनाकर अपना भोजन पैदा कर रहे थे। उन्होंने वहीं बसने का निश्चय किया।
वे उन नई धराओं पर बस गए, जिन्हें अनगिनत नदियों ने सींचा था। आज भी धरती उन उथल-पुथल वाले समय के कठोर प्रमाण उगल रही है, जहाँ बसी-बसाई बस्तियाँ नष्ट हो गईं, और उनकी जगह लेने के लिए नई लेकिन अस्थिर भीड़ आ गई।
मेहनत से बसाई गईं बस्तियाँ नष्ट कर दी गईं, और उनकी यादें बस धूल और सन्नाटे में खो गईं। देवताओं ने दस्युओं को मिटा दिया, और वेद उन रक्तरंजित घटनाओं के वर्णन से भर गए।
इतिहास कहता है कि वाराणसी भी अपने हिस्से के दुख से बच नहीं सकी। लेकिन वाराणसी ने कभी भी धूल में सिमटने से इनकार कर दिया। बार-बार लूटी गई, फिर भी वह बार-बार उठ खड़ी हुई।
वह पुरानी दादी की तरह है, जो अपने अनुभवों की गठरी लिए हुए है, और हर उथल-पुथल को सतही हलचल मानकर मुस्कुराती है। वह धूल और मलबे के ढेर में से सिर उठाकर खड़ी होती है — लहूलुहान, पर अडिग।
उसे खुशी है कि वह अपने टूटे-फूटे ढाँचे के बावजूद अपनी आत्मा को बचाए रखने में सफल रही। वह, जो माताओं की भी नानी है, हर बदलाव को अपनी पुरानी शाल में लपेट लेती है — धर्मों और संस्कृतियों की बदलती बुनावट के साथ, और फिर भी, हमेशा की तरह, अपने अंतहीन, शांति भरे दैनिक जीवन में लौट आती है।
इतिहास गुजरता है, लेकिन वाराणसी मुस्कुराते हुए समय की हर चुनौती से उबर जाती है।
काल भैरव, 'भयावह समय', इस अमर शहर का संरक्षक है।
अन्य प्राचीन नगरों की धड़कन शायद ही हमें महसूस होती है, लेकिन वाराणसी की उपस्थिति हमें झकझोर देती है। यह शहर समय के चेहरे पर एक विद्रोह है — एक अमर आत्मा जो काल के सामने कभी नहीं झुकती।
लेकिन त्रासदी यह है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, जब श्रद्धा मुरझा रही है, विश्वास विलुप्त हो रहा है, और आत्मा एक अधूरा स्वप्न बन गई है।
आधुनिक यांत्रिक व्यवस्था के तीव्र और अकारण प्रहारों से मानवता अपने ही बनाए खंडहरों के बीच ठिठकी खड़ी है, उजड़े सपनों के मलबे में एक रोशनी की तलाश कर रही है।
हम एक ऐसे भगवान को खोजते हैं, जो है ही नहीं। हम एक ऐसी वाराणसी को खोजते हैं, जो है भी, और नहीं भी।
हम एक खोई हुई आस्था की खोज में निकलते हैं, और हमारी टूटी-फूटी आशाएं फिर से वाराणसी के नाम पर पुनर्जीवित होती हैं।
वाराणसी ने अपनी आत्मा को खोया नहीं है, चाहे वह कितनी भी बार उजाड़ी गई हो।
क्योंकि वाराणसी की खोज, दरअसल हमारी अपनी आत्मा की अंतिम खोज है।
II
हम एक समुदाय के सदस्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से प्राचीन परंपराओं से जुड़ जाते हैं। हमारा अतीत हमारा आधार, हमारी जड़, हमारा विश्वास, हमारा कवच और कभी-कभी हमारा पलायन होता है। हमारा अतीत एक ऐसा स्वप्नलोक है, जहाँ हम बार-बार लौटना चाहते हैं।
लेकिन वाराणसी केवल एक आस्था या पलायन का साधन नहीं है। यह उतनी ही दृढ़ है जितनी एक जीवित आस्था। यदि हमें जीवन को सही मायने में जीना है, तो कम से कम एक बार हमें अपनी धड़कनों में वाराणसी की प्राचीन आत्मा को महसूस करना ही होगा।
वाराणसी के नाम में शांति और तर्क, प्राचीनता और आधुनिकता, कट्टरता और उदारता एक साथ समाहित हैं। अकेलापन और भीड़, पवित्रता और भय, उत्थान और पतन, जिद और ढीलापन — ये सब वाराणसी में एक साथ सांस लेते हैं। वाराणसी समय की एक सराय है।
प्रेम की तरह, वाराणसी ने भी उतार-चढ़ाव देखे हैं — नया और पुराना, सपना और जागृति, आस्था और संशय, जीवन और मृत्यु, वादा और विश्वासघात।
आधुनिक जीवन की शांति और सादगी के लिए जो कीमत चुकानी पड़ रही है, वह बहुत भारी है — क्योंकि जीवन ने अपनी मूल मूल्यवत्ता खो दी है। जीवन बहुत सस्ता हो गया है।
लेकिन क्या खंडहरों में ही सब सपनों की अंतिम परिणति नहीं होती? क्या धार्मिक उत्साह का चरम बिंदु कभी-कभी व्यंग्य और कटुता में नहीं बदल जाता? खंडहर खोजने के लिए ललचाते हैं, खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या खोज वास्तव में आवश्यक है? होमर के ओडिसियस की तरह, अंततः यह समझ में आता है कि खोजने के लिए शायद कुछ बचा ही नहीं है — मनुष्य और प्रकृति मूल रूप से अपरिवर्तित ही रहते हैं।
फिर भी, वाराणसी खोज की मांग करती है। वाराणसी को खोजने का अर्थ है मानव धरोहर को खोजना। क्योंकि सभी प्राचीन मानव सभ्यताओं में, केवल वाराणसी ही है जो आज भी जीवित है, धड़क रही है, और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है।
क्यों?
क्योंकि वाराणसी में अच्छाई और बुराई इतनी गहराई से मिल गई हैं कि शुद्ध मूल्यों को अलग करना कठिन है, बिना प्राचीन आस्थाओं और विश्वासों के उलझे हुए धागों से टकराए।
वाराणसी का लंबा इतिहास कई उजड़े भविष्य की कहानी कहता है। उसकी प्रसिद्धि की स्थायित्व लोगों की उस आस्था पर टिकी है, जो मूल्यों की वास्तविकता में विश्वास रखती है।
विचारों की आत्मिकता में एक अनूठा आकर्षण होता है। यह हमें आस्था और विश्वास के जटिल खेल पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। और यही विचार हमें जीवन में शांति की खोज में मूल्यों की भूमिका को समझने की ओर ले जाता है।
वाराणसी आज भी शांति की गारंटी देती है — मानवता की अंतिम तलाश।
इन विरोधाभासी लेकिन सम्मोहक पहलुओं के बीच, वाराणसी — अनंत, अविनाशी — अपनी निरंतरता की अमरता को बनाए रखती है। यह एक ऐसा संदेश देती है, जो आज भी बीमार और उत्साही, विक्षिप्त और ध्यानमग्न, निराश और तिरस्कृत, विद्वान और धार्मिक, आदर्शवादी और सनकी लोगों को आकर्षित करता है।
इसीलिए वाराणसी आज भी एक पर्यटक की अनिवार्य मंज़िल और एक तीर्थयात्री की अंतिम आशा बनी हुई है। यह एकांतप्रिय साधु के लिए आश्रय है, और विचित्र लोगों के लिए एक आकर्षक भटकन।
वाराणसी के तंग, गंदी गलियों में बेतरतीब भीड़, सड़ांध मारते फूलों और खाने की थालियों के बीच बहुरूपी जीवन चलता है। हर मोड़ पर बिल्लियाँ, कुत्ते, गाय और अपराधी बेखटके पंडितों, भिखारियों, राजाओं और वेश्याओं के साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं।
किसी मोड़ पर कोई ठग नाटक कर रहा होता है, कोई शोकाकुल रो रहा होता है, एक बैल मस्त चाल से गुजर रहा होता है, या कोई पागल आदमी अश्लील बातें चिल्ला रहा होता है। एक शवयात्रा गुजरती है, जबकि दूसरी ओर एक शादी की बारात ढोल-नगाड़ों के साथ नाचती हुई निकलती है। दीवाने फकीर अपनी जादुई धुन गाते हैं, शोकग्रस्त विधवाएँ अपनी करुणा भरी आवाज में विलाप करती हैं। और वहीं, गर्मागरम समोसे बेचने वाला निश्चिंत होकर अपनी पुकार लगाता है।
पुराने और उलझे हुए वाराणसी के अतीत और भ्रमित वर्तमान में मानवीय मूल्यों की टकराहट होती रहती है। आध्यात्मिक, त्यागी, मुक्तात्मा लोग गंदी, बीमार, भिखारी, और पागल लोगों के साथ एक ही नदी में स्नान करते हैं।
लिंग, उम्र, संप्रदाय और धार्मिक भिन्नताएँ गंगा की अविरल धाराओं में बहकर मिल जाती हैं — ठंडी, गहरी, शाश्वत और आदि।
वाराणसी ही गंगा है, और गंगा ही वाराणसी।
वाराणसी उत्थान देती है, और अवसाद भी। वाराणसी मुक्त है, और कभी-कभी विक्षिप्त भी।
भारी भरकम बैल, बेपरवाह गधे, अपमानित कोढ़ी, मज़ाकिया बंदर, कुंडली मारकर बैठे सांप, भविष्य बताने वाले ढोंगी, और मिन्नतें करते भिखारी — सभी वाराणसी की गलियों में बेपरवाही से गुजरते हैं।
वाराणसी हर रूप को ठुकरा देती है।
वाराणसी जन्म से ही बूढ़ी थी। उम्र ने उसे कभी छोड़ा नहीं, और युवावस्था ने उसे कभी छुआ नहीं। समय उसे मुरझा नहीं सका, और खुलापन उसकी आत्मा से कभी छीना नहीं जा सका।
न तो किसी चित्रकार की कूची ने उसकी नदी के रहस्यमय सौंदर्य को छुआ, न ही कैमरों ने उसकी आत्मा को बाँध पाया।
समय उसे कभी बासी नहीं बना सका, न ही उसकी तीखी, चटपटी ऊर्जा को मिटा पाया।
वाराणसी की जादुई शक्ति आज भी एक कठोर शहरी निंदक, एक सबकुछ जानने वाले पुरातत्वविद, एक दार्शनिक, एक विद्वान, एक संत, एक साधक, एक नृत्यांगना, और एक प्रबुद्ध संत को समान रूप से मोहित करती है।
वाराणसी में रहना समय के एक कैप्सूल में बंद होने जैसा है, मानो कोई आध्यात्मिक चलचित्र चल रहा हो।
इन तमाम पहलुओं के ऊपर, वाराणसी के आसमान में एक अदृश्य लेकिन प्रबुद्ध देवदूत की तरह धर्म और भक्ति की रोशनी टंगी रहती है।
वाराणसी की तस्वीरें: पर्यटकों के रेखाचित्र
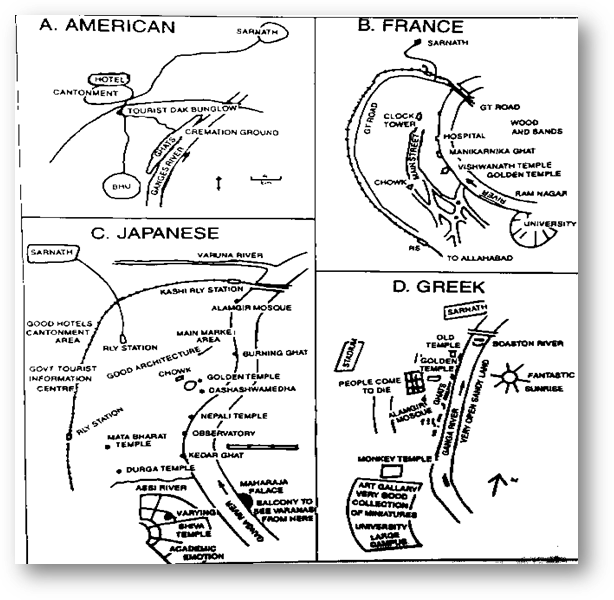 मानचित्र 2. वाराणसी के
पर्यटकों के रेखाचित्र: अमेरिकी, फ्रांसीसी, जापानी और ग्रीक
मानचित्र 2. वाराणसी के
पर्यटकों के रेखाचित्र: अमेरिकी, फ्रांसीसी, जापानी और ग्रीक
क्योंकि, चाहे कुछ भी कहा जाए, मनुष्य की आत्मा को राहत देने की उसकी अनिवार्य भूख उतनी ही सच्ची है जितनी उसकी पीड़ा।
जब तक मनुष्य को अस्तित्व की आवश्यकता होगी, तब तक वह किसी न किसी रूप में धर्म की खोज करता रहेगा।
धर्म, वास्तव में, अकेले व्यक्ति का अंतिम साथी है।
और वाराणसी, अपनी भीड़ भरी तन्हाई में, एक साधु के लिए वैसी ही है जैसी किसी योगी के लिए उसकी गुफा।
III
वाराणसी की स्वाभाविक जिद उसे पतन के अपमान के आगे झुकने नहीं देती। वह अन्य प्रागैतिहासिक नगरों की तरह बिखरने से इनकार करती है। हर आक्रमण के बाद वह अपने कौमार्य को फिर से पा लेती है। वह विनाशों को गौरवशाली स्मारकों में बदल देती है, और विश्वास की एक नई परत जोड़ लेती है। हर घाव उसे और भी मजबूत बनाता है, हर गिरावट उसे और ऊर्जावान बना देती है। मंदी उसे फिर से संजोती है; बाढ़ उसे उर्वर बनाती है; मृत्यु उसे पुनर्जन्म देती है।
उसकी अविश्वसनीय नदी किनारे की सुंदरता ने कवियों को छंद गढ़ने, कलाकारों को चित्र बनाने, संगीतकारों को गाने और फोटोग्राफरों को आश्चर्य से भरकर कैमरा उठाने के लिए प्रेरित किया है।
जो वाराणसी ने टर्नर (प्रसिद्ध चित्रकार) के न होने में खोया, उसे उसने अपने विनम्र पर सच्चे चित्रकारों की टोली में पा लिया। वाराणसी की तंग गलियों में रहने वाले ये साधारण चित्रकार कभी निष्क्रिय नहीं रहे।
वाराणसी के पास कोई स्ट्रॉस (संगीतकार) नहीं है जो गंगा के लिए एक "ब्लू-गंगा" रचे, लेकिन गंगा के गीत यहाँ तब से गाए जा रहे हैं, जब संस्कृत भी उतनी प्राचीन नहीं थी। वेदों ने सिंधु और सरस्वती की स्तुति की, लेकिन पाली और प्राकृत ने गंगा की महिमा गाई — उस गंगा की, जो पतितों की पावनी है, जो स्वर्गीय धारा है, और जिसने वैदिक अहंकार को भी तोड़ा।
भारत के किसी भी अपभ्रंश भाषा परिवार ने गंगा की महिमा गाने से खुद को वंचित नहीं रखा है। हम हैरान और गर्वित होते हैं जब हमें पता चलता है कि "गंगा" शब्द की जड़ एक भाषा से है, जो भारत की मूल संपर्क भाषा थी — मुंडारी।
वैदिक संस्कृत के अपने अभिजात्य प्रभुत्व के पहले, 'गंगा' का अर्थ मुंडारी में वही था जो आज है — 'नदी'।
महाभारत में एक कथा कहती है कि वैदिक आर्यों के सबसे प्रसिद्ध वंशों की उत्पत्ति एक "गंगा-कन्या" के गर्भ से हुई, जो संभवतः एक गैर-आर्य, शायद एक अनाम मुंडारी महिला थी। भारत के मूल निवासी समुदाय — जैसे मुंडा, भरा, सुइर, कोल, हो, बिरोर, गोंड — सभी को नागा, द्रविड़ या दस्यु के व्यापक नाम के तहत जाना जाता था।
इनमें से अधिकांश पूर्व-वैदिक भाषाओं में गंगा और वाराणसी पर गीत गाए गए हैं। सबसे मार्मिक गीतों में से कुछ इस्लामी कवियों द्वारा रचे गए हैं।
जबकि गंगा और वाराणसी पर गीत आज भी सभी भारतीय भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं, समय की मार के कारण चित्रात्मक रिकॉर्ड दुर्लभ हैं। लेकिन मूर्तियों के साथ ऐसा नहीं है। गंगा को पत्थर और टेराकोटा में बार-बार उकेरा गया है। सबसे उल्लेखनीय उदाहरण महाबलीपुरम और एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं।
फिर भी, वाराणसी और उसके कलाकारों ने चित्रकला की परंपरा को जीवित रखा। पुराने समय के अधिकांश वाराणसी कलाकार, और आज के भी, अपनी मिट्टी की दीवारों पर चित्र बनाने के जुनून से भरे हुए हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है।
लेकिन जहाँ फ्रांस की सरकार ने ताहिती की मिट्टी की दीवारों की चित्रकला को सहेजने के लिए अथक प्रयास किए, वहीं वाराणसी की दीवारों पर बनी अद्भुत कलाकृतियों को बेरहमी से भुला दिया गया।
अभिजात्यवाद और नौकरशाही की ठंडी उदासीनता मिलकर किसी भी कला रूप की सबसे प्रभावी हत्यारे बन जाती हैं।
कुछ आधुनिक कलाकारों ने वाराणसी के अद्वितीय परिदृश्य को सहेजने की कोशिश की। एक अनजान सैनिक, जो 1765 में सर रॉबर्ट फ्लेचर की सेना में था, ने पूर्वी तट से वाराणसी के दृश्य का एक बेहद कीमती चित्र छोड़ा है।
1831 में सर जेम्स प्रिंसेप ने अपनी कलम और कूची से वाराणसी के जीवन की झलक को अमर कर दिया।
ये अमूल्य चित्र वाराणसी को मुग़ल काल के अंत में जैसा था, वैसा दिखाते हैं। फ्लेचर का चित्र इंग्लैंड में गुमनाम पड़ा रहा, शायद चित्रकार ही इसे ले गया था।
भारतीय ऐतिहासिक समाज को जब इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे हासिल किया। आज यह चित्र कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय की दीवार पर टंगा है — गर्व की एक अमूल्य धरोहर की तरह।
IV
क्या
बस इतना ही है?
क्या वाराणसी का और कोई प्रागैतिहासिक अस्तित्व नहीं है?
वाराणसी ने अपनी यात्रा उस इतिहास के बहुत पहले शुरू की होगी, जिसे
हम 'उपलब्ध अभिलेखों' के रूप में जानते हैं। वह तब भी जीवित थी,
जब हड़प्पा और कालीबंगन के मिट्टी के निर्माता आर्यों के आगमन के बारे में नहीं जानते थे।
उन विनाशकारी घटनाओं के रिकॉर्ड, जहाँ एक जाति ने दूसरी जाति को पूरी तरह पराजित और अपमानित किया, ऋग्वेद की ऋचाओं, कुछ सामाजिक मानदंडों और ब्राह्मणवादी परंपराओं के माध्यम से व्यक्त हुए हैं।
महाभारत हमारे लिए एक अमूल्य स्रोत है, जो इस पराजय की कथा को दर्शाता है — अधिकारों, संपत्ति, स्त्रियों और धार्मिक परंपराओं की लूट से लेकर, दासों और बंधुआ मजदूरों (दास) के एक सामाजिक वर्ग की रचना तक। आर्यों के बीच महिलाओं की कमी को कैद की गई महिलाओं को उपहार के रूप में प्रस्तुत करके पूरा किया जाता था।
"किसी भी महिला से जन्मा बच्चा यदि आर्य पुरुष का था, तो वह आर्य कहलाता था," यह उस समय के कानूनों में लिखा गया।
लेकिन यह भूल होगी कि हम महाभारत को उसकी वर्तमान स्वरूप में पूरी तरह सत्य मान लें। क्योंकि वर्षों की छेड़छाड़ और परिवर्तन के कारण मूल कथा को बार-बार बदला गया। खासकर भार्गवों (एक विद्वान समूह) द्वारा, जिन्हें आर्यों के महिमामंडन के लिए नियुक्त किया गया था, मूल निवासियों को हाशिए पर धकेलने की कीमत पर।
हमें संदेह होता है — क्या ये ग्रंथ सचमुच खो गए थे? या जानबूझकर मिटा दिए गए?
इस संदर्भ में, हमें कृष्ण द्वैपायन व्यास (महाभारत के रचयिता) के एक शिष्य याज्ञवल्क्य का उल्लेख करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने आर्यों की सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध विद्रोह किया। वह व्यास की पाठशाला छोड़कर एक नई अकादमी स्थापित करने निकल पड़े, जिसमें उन्होंने 'जनजातीय' विद्यार्थियों को शिक्षित किया। ये थे 'तित्तिर' — एक पक्षी टोटम को मानने वाली जनजाति।
याज्ञवल्क्य ने 'याज्ञवल्क्य सामाजिक संहिता' की रचना की, जो मनु, अत्रि, विष्णु, हरित और गौतम (बुद्ध नहीं) जैसे प्राचीन कानून-निर्माताओं की संहिताओं के विरुद्ध थी।
यह इस बात का प्रमाण है कि तब भी, जब महाकाव्य की नींव रखी जा रही थी, ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही थीं।
पुरातात्विक खोजें भी बताती हैं कि वाराणसी क्षेत्र में पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, और खिलौने मिले हैं, जो 14 परतों तक नीचे पाए गए। यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ गैर-आर्य जनजातियाँ बसी थीं।
आज भी वाराणसी की भाषा, जीवन शैली, और सांस्कृतिक व्यवहार में उस गैर-आर्य स्वतंत्रता की झलक मिलती है। 'बनारसी अंदाज़' दरअसल एक अनौपचारिक, मस्तमौला, 'जैसा है वैसा ही सही' जीवन दृष्टिकोण है, जो भंडा, भरा, सुइर, अविर जैसी जनजातियों से आया है।
यही वजह है कि भैरव, शैव और तांत्रिक परंपराएँ काशी के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हैं। विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है कि यह क्षेत्र शिव के प्राचीन अनुष्ठानों का केंद्र रहा है।
महाभारत की एक और दिलचस्प कथा है — एक पशु-शीर्ष वाले गण-देवता को व्यास का लिपिक नियुक्त किया गया। विद्वानों का मानना है कि यह कथा संभवतः एक बाद की मिलावट है, जो स्थानीय जनजातियों की भागीदारी को दर्शाती है।
इस संदर्भ में गणेश को वास्तव में यक्ष राजा कुबेर का एक रूप माना जाता है — जो शिव की विरासत की रक्षा के लिए खड़े थे।
इससे पता चलता है कि ब्राह्मणवादी हस्तक्षेप को चुनौती दी गई थी।
हम यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि खोई हुई 'जया' में गैर-आर्य सभ्यता की गौरवशाली कहानियाँ थीं। यदि वे कथाएँ बची होतीं, तो क्या हड़प्पा संस्कृति और उसकी लिपि आज भी एक रहस्य बनी रहती?
आर्यों के आक्रमण, और स्थानीय संस्कृति की महानता को उस ग्रंथ से मिटा दिया गया।
महाकाव्य को फिर से लिखा गया, ताकि नए विजेताओं की वीरता का बखान किया जा सके — जो स्थानीय महिलाओं को अपनाकर, अपने कबीले को बढ़ाने में नहीं हिचकिचाते थे। मत्स्यगंधा, परमलोचना, गंगा, अंजना, कुंती, हिडिंबा, जांबवती — ये सभी महिलाएँ इस 'मिश्रण' की गवाह थीं।
जाति-प्रथा का आधार भी इन्हीं अंतर्जातीय विवाहों में देखा जा सकता है। जाति-प्रथा का तर्क, रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए, यथार्थ से परे और अस्वीकार्य लगता है। लेकिन ब्राह्मणवाद को शीर्ष पर बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था बेहद कारगर साबित हुई।
सच कड़वा है, लेकिन उसे नकारा नहीं जा सकता।
सैकड़ों लोककथाएँ, दंतकथाएँ, कहानियाँ हमें उन नगरों, गाँवों और लोगों की दुखद याद दिलाती हैं, जिन्हें नष्ट करके, विजेताओं ने अपनी सत्ता स्थापित की।
खांडव वन का दहन, जनस्थान का विध्वंस — ये सब आर्य शांति की कथाओं को झुठलाते हैं।
लेकिन जब युद्ध की धूल बैठ गई, और खून की नदियाँ धरती को उपजाऊ बना गईं, तब भी वाराणसी अपनी जगह पर डटी रही — अडिग, अटल।
कोई भी आर्य आक्रमण वाराणसी को नहीं हिला सका। गणेश, भैरव, कालभैरव — ये सभी वाराणसी की सीमाओं की रक्षा करते रहे। काशी के विभिन्न गणेश और भैरव मंदिर आज भी इस इतिहास की जीवित गवाही देते हैं। पौराणिक ग्रंथों और हिंदू धर्मशास्त्रों में इस संघर्ष के अनेकों संदर्भ मिलते हैं। आर्यों की आंधी के खिलाफ, इस उपमहाद्वीप के स्वदेशी लोग लड़ते रहे।
विजेताओं ने स्थानीय देवताओं को बदलने की कोशिश की — नदियाँ, पहाड़, पेड़, और पूर्वजों की आत्माएँ — इन सबकी पूजा को 'अधर्म' घोषित किया गया।
लेकिन आखिरकार, 80% से ज्यादा जो आज हिंदू धर्म कहलाता है, वह इन विजित लोगों की परंपराओं का ही रूपांतरित संस्करण है।
हिंदू धर्म, वास्तव में, 'सिंधु धर्म' का ही एक नया स्वरूप है।
और जब हम हिंदू धर्म की सतह को खरोंचते हैं, तो उसके नीचे वही गैर-वैदिक, स्वदेशी परंपराएँ मिलती हैं, जो हजारों सालों से वाराणसी की आत्मा को जीवित रखे हुए हैं।
V
इस निरंतर क्षरण के बीच भी वाराणसी वहीं बनी रही, जहाँ वह सदियों से है। गंगा के किनारे, शांति और आत्म-संयम के साथ, वह थके हुए को सांत्वना देती है, सताए हुए की रक्षा करती है, शरणागत को आश्रय देती है, बीमार को शुद्ध करती है, और व्याकुल को संतुलित करती है।
वेन्स, फ्लोरेंस, जिनेवा या लुसेर्न की बात करें, या टेम्स से लंदन के दृश्य की, न्यू जर्सी की पहाड़ियों से न्यूयॉर्क की छवि, या नदी के उस पार से एडमंटन का दृश्य — कोई भी नदी किनारे का नगर वाराणसी की सुंदरता और भव्यता की बराबरी नहीं कर सकता। जैसे इमारतों के बीच ताजमहल, या संगमरमर की मूर्तियों में वीनस डी मीलो, उसी तरह वाराणसी की सुंदरता एक अनुभूति है, एक आत्म-बोध है, एक संवेदना है, जिसे केवल एक सच्चा सौंदर्य-प्रेमी ही महसूस कर सकता है।
वर्ड्सवर्थ ने लिखा था — "पृथ्वी पर इससे सुंदर कुछ नहीं है।" शायद इसलिए, क्योंकि उन्होंने कभी गंगा के किनारे से वाराणसी को एक सर्द सुबह के उगते सूरज की हल्की किरणों में नहीं देखा था।
वाराणसी के मोहपाश को तोड़ने और अपने मन को शांत रखने के लिए अद्भुत संकल्प और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है जैसे सदियों की भूली हुई परेड पत्थरों और मंदिरों के मीनारों से धीरे-धीरे रिस रही हो। पीतल की घंटियाँ किसी अनजानी दिशा से गूँजती हैं, उनकी ध्वनियाँ लहरों की तरह वापस लौटती हैं।
तीर्थयात्री एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वातावरण में ऐसा लिपट जाता है, जैसे कोई शौकिया पर्यटक रोम, वेनिस, फ्लोरेंस या साल्ज़बर्ग की सँकरी गलियों में खो जाता है। वाराणसी अपने प्रागैतिहासिक अस्तित्व के भार से अभिभूत कर देती है।
यहाँ की गंदगी, सड़ांध, सदियों पुरानी चालाकी और धोखेबाजी की परंपरा, पुरोहितों की लालच और भिक्षावृत्ति का समय-सम्मानित चक्र, अजीबो-गरीब गंध, चटख रंगों से भरी भीड़, और धरती के परित्यक्त, गलते हुए शरीर — सब एक साथ मन पर हावी हो जाते हैं।
दर्शनिक बैल, मुँह चिढ़ाते बंदर, दिखावे के अजगर और नाग, भविष्य बताने वाले पक्षी, और इंसान-जानवर के अद्भुत सह-अस्तित्व के बीच संघर्षरत जीवन — ये सब मानसिक दृढ़ता की अंतिम परीक्षा लेते हैं।
यहाँ की पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई जल्दी से पीछे हटकर परिचित, आरामदायक माहौल में लौट जाना चाहे, लेकिन वह लौट भी जाए, तो यह शहर उसे फिर से खींच लाता है। ऐसा लगता है जैसे इस जगह की यादें एक अजीब, कठोर वास्तविकता में रोमांस की तलाश में बार-बार बुलाती हैं।
केवल सबसे साहसी लोग ही इस तेजी से बदलते समय के चक्रव्यूह में टिक सकते हैं।
परिचित और अपरिचित, अतीत और वर्तमान, इतिहास और जीवन के इस अप्रत्याशित मिश्रण से अप्रशिक्षित मन चौंक जाता है — जैसे भूतिया नृत्यों और दिव्य अनुभवों के बीच लगातार झूल रहा हो।
वाराणसी एक पर्यटक के लिए चुनौती है, एक तीर्थयात्री के लिए मानसिक परीक्षा, एक कवि के लिए प्रेरणा की डायरी, और एक आवारा के लिए स्वर्ग है।
यह इंसान की त्वरित अनुकूलन क्षमता का विस्तार है।
वाराणसी एक कला एलबम है, अजीबोगरीब चीजों का संग्रहालय है, एक स्वच्छता निरीक्षक की नोटबुक है, और एक भोजन-प्रेमी के लिए स्वर्ग है।
वाराणसी उन मानसिक रूप से पीड़ितों का अंतिम आश्रय है, जो अपने भीतर एक गहरा अकेलापन महसूस करते हैं।
"येषाम् अन्य गतिर्नास्ति, तेषाम् वाराणसी गतिः।"
"जिनके लिए कोई और मार्ग नहीं बचा, उनके लिए वाराणसी ही अंतिम गंतव्य है।"
यहाँ, जो व्यर्थ लगता है,
वह दिव्यता को छू लेता है। और एक ज्ञानी, आत्म-खोज की उस वांछित शांति तक पहुँच जाता है, जिसे
वह अनगिनत जन्मों से तलाश रहा था।
2.बदलता हुआ परिदृश्य
I
जब
हम वाराणसी की बात करते हैं, तो
क्या हमें सच में पता है कि यह शहर वास्तव में कहाँ स्थित है?
क्या वाराणसी हमेशा से एक शहर थी?
अगर नहीं, तो उसे यह दर्जा कब मिला?
फिर, काशी कहाँ है?
यह भी एक ज़रूरी प्रश्न है।
क्या काशी और वाराणसी एक ही हैं?
या फिर वे दो जुड़वां शहर हैं,
जैसे हावड़ा-कलकत्ता, या सेंट पॉल-मिनियापोलिस?
पुराणों और जैन-बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, काशी और वाराणसी दो अलग-अलग स्थान प्रतीत होते हैं। वाराणसी एक पवित्र पहाड़ी थी, जो घने जंगलों से ढकी थी, कई नदियों और जलधाराओं से धुली हुई थी, और बड़े-बड़े जलाशयों से सजी हुई थी।
वाराणसी प्राचीन काशी-कोशल जनपद की एक सशक्त, दुर्गम राजधानी थी।
काशी
और वाराणसी के अलावा,
हमें चार अन्य नामों का भी उल्लेख मिलता है: आनंदकानन,
गौरीपीठ, रुद्रवास और महाश्मशान।
अब प्रश्न यह उठता है — इन स्थानों की पहचान और अवस्थिति कहाँ की जा सकती है?
यदि ये स्थान अलग-अलग हैं, तो
कौन-सा सबसे पुराना है?
अगर ये सभी ऐतिहासिक वास्तविकताएँ हैं, तो
हमारा यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है।
जातक कथाओं में हमें काशी के और भी कई नाम मिलते हैं।
लेकिन उन पर हम धीरे-धीरे चर्चा करेंगे।
या क्या हम इन नामों को महज़ मिथक मानकर खारिज कर सकते हैं?
लेकिन मिथक भी पूरी तरह अवास्तविक या निराधार नहीं होते।
जो पूरी तरह असत्य होता है, वह
पचास शताब्दियों तक जीवित नहीं रह सकता।
ग्रेव्स और गोपीनाथ कविराज के अनुसार, मिथक इतिहास के ही छिपे हुए रूप होते हैं, जो प्रतीकात्मक भाषा में संरक्षित किए जाते हैं, ताकि वे आम जनता को शिक्षित कर सकें।
मिथक समाजशास्त्र के छात्रों के लिए एक सांस्कृतिक 'माइंड-बैंक' की तरह काम करते हैं।
II
प्राचीन वाराणसी के स्थल की खोज के लिए हमें उन सभी संदर्भों और पुरातात्विक अवशेषों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा, जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध हैं। हमें वेद, संहिताएँ, जैन-बौद्ध ग्रंथ (विशेष रूप से जातक कथाएँ), पुराण, महाकाव्य, यात्रियों के वृत्तांत, लोककथाएँ, और निश्चित रूप से आज भी मौजूद खंडहरों और स्मारकों का बारीकी से अध्ययन करना होगा।
वह वाराणसी, जो संन्यासियों, ऋषियों और आध्यात्मिक खोजियों के लिए पवित्रतम स्थान थी, कभी एक पहाड़ी वनभूमि थी, जो जीवन की आपाधापी से दूर, शांति से छिपी हुई थी।
यह स्थान हमेशा से वहीं था, और इसे स्थानीय आदि-निवासी समुदाय जानते थे — वे समुदाय जो आर्यों के आगमन से पहले से इस भूमि के मूल निवासी थे। नृविज्ञान (एंथ्रोपोलॉजी) में इन्हें 'द्रविड़' कहा गया, जबकि वैदिक साहित्य में इन्हें दस्यु, दानव, नाग, असुर, यक्ष और राक्षस के नाम से पुकारा गया।
महाकाव्यों और पुराणों में इन्हें 'गण-नाग' के समग्र नाम से भी संबोधित किया गया है।
वाराणसी उन नाग और द्रविड़ समुदायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो लिंग-पूजा करते थे और जिन्हें स्थानीय स्तर पर भरा, भंडा, और सुइर के नाम से जाना जाता था।
आर्यों के वाराणसी के बारे में जानने से बहुत पहले ही नागों और गणों ने इस स्थान के प्रति गहरा सम्मान रखा था।
III
आर्यों का आगमन एक रहस्यमय घटना थी। 'एयरयास' (अवेस्ता ग्रंथों में), या एशिया माइनर के भूले हुए हित्ती समुदाय से जुड़े ये आर्य, किसी अज्ञात कारण से एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों की ओर बढ़े। इन इंडो-आर्य कबीलाई समूहों ने हिंदुकुश की दुर्गम पर्वत श्रृंखला को पार किया।
सिंधु नदी की विशालता ने उन्हें चौंका दिया और उन्होंने इसकी महिमा की प्रार्थना शुरू कर दी। यह घटना संभवतः 5500 वर्ष पहले घटी होगी।
आर्य कई अलग-अलग समूहों में आए — जैसे मद्र, परस, शाक, भरत, कश्यप, वास, तुरवस आदि। उन्होंने 'पंजाब' (पाँच नदियों की भूमि) में बसने की कोशिश की।
भारत में उनके आगमन की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है — कुछ इसे 3500 ईसा पूर्व मानते हैं, तो कुछ 2500 ईसा पूर्व।
उन्होंने पहले सिंधु घाटी में बसने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की परिष्कृत और उन्नत सभ्यता ने उनके आक्रमण को गंभीर चुनौती दी।
2500 ईसा पूर्व तक, स्थानीय संस्कृति आर्य आक्रांताओं के अधीन हो गई।
हालाँकि, वे लंबे समय तक सिंधु और सरस्वती की घाटियों में बसे रहे। लगातार वनों की कटाई के कारण उन्होंने उस क्षेत्र को रेगिस्तान में बदल दिया, और सरस्वती नदी रेत में समा गई।
वे धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़े, जब तक कि वे मध्य भारत की हरी-भरी घाटियों — विशेष रूप से गंगा और यमुना (सदानिरा, गंडकी) के पास नहीं पहुँच गए।
लेकिन उनका यह विस्तार कभी भी बिना संघर्ष के नहीं हुआ।
स्थानीय निवासियों — जिन्हें वे तिरस्कारपूर्वक असुर, दस्यु, दानव, राक्षस और यक्ष कहते थे — ने घोर प्रतिरोध किया।
ऋग्वेद में भी इन स्थानीय समुदायों की उन्नत संस्कृति का उल्लेख है।
इनमें से सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र, जिसे स्थानीय लोग सबसे अधिक प्यार करते थे, वह था वाराणसी के वनाच्छादित पर्वत।
ये घने जंगल और बाग-बगीचे — जिनका वर्णन काशीखंड (स्कंदपुराण) में मिलता है — गंगा के किनारे बसे थे, और असि, गोदावरी, मंदाकिनी, धूतपापा, किरणा और वरुणा नदियों से सिंचित थे।
स्थानीय लोगों को यह क्षेत्र एक सजीव स्वर्ग जैसा लगता था, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से अपने पशुपति और माता देवी की पूजा करते थे।
वेदों को 'माता' या पुरुष-प्रकृति के संतुलन की कोई समझ नहीं थी। इसलिए वे इस प्रकार की पूजा को 'रुद्र' (भीषण) पूजा कहते थे। उन्होंने इन रहस्यमयी पहाड़ियों को 'रुद्रवास' (रुद्रों का निवास) या 'महाश्मशान' कहा — एक ऐसा स्थान, जहाँ की अजीबोगरीब अंत्येष्टि परंपराओं के कारण, यह एक विशाल श्मशान जैसा प्रतीत होता था।
ऋग्वेद में रुद्रों को 'अवैदिक' कहा गया है। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में, वेदिक और रुद्र परंपराओं के सह-अस्तित्व का उल्लेख मिलता है।
'रुद्रवास' नाम शायद इन्हीं घटनाओं की याद दिलाता है।
'महाश्मशान' नाम संभवतः गंगा तट और पहाड़ियों के किनारे फैले विशाल श्मशान स्थलों की ओर संकेत करता है, जहाँ मांसाहारी, भीषण लोग रहते थे, जिन्हें आर्य समाज नकारता था।
वेद और पुराणों में इस संघर्ष की पुष्टि होती है।
वाराणसी ने तब भी, और आज भी, 'रुद्र परंपराओं' को जीवित रखते हुए एक सख्त 'अवैदिक' रुख अपनाया है।
इसलिए, वाराणसी निश्चित रूप से वैदिक युग से पहले की है। आर्यों ने इसे एक पवित्र स्थान के रूप में बहुत बाद में स्वीकार किया — नैमिषारण्य, द्वैतवन, काम्यकवन, पुष्करावती, सरस्वती और कुरुक्षेत्र के बाद।
लेकिन वाराणसी ने अपने आरंभिक अस्तित्व को कभी नहीं खोया।
यहाँ तक कि जब आर्य धीरे-धीरे वाराणसी में बसने लगे, तब भी स्थानीय परंपराएँ गहरी जड़ों के साथ कायम रहीं।
वाराणसी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं थी — यह एक जीवंत परंपरा थी, जो आक्रमणों, संघर्षों, और सांस्कृतिक विलयों के बावजूद अपनी आत्मा को बचाए रखने में सफल रही।
IV
काशी
नगर बार-बार युद्धों और धार्मिक कट्टरता की लड़ाइयों में पूरी तरह नष्ट हो गया था।
1194 ईस्वी में मुहम्मद गोरी और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के हमलों के बाद, कन्नौज
और काशी केवल धुंधली यादें बनकर रह गए थे।
लेकिन कन्नौज और काशी जैसे व्यापारिक नगरों के आर्थिक महत्व ने व्यापारिक समुदाय को मजबूर कर दिया कि वे इन क्षेत्रों के आसपास नए, उपयुक्त केंद्रों की तलाश करें।
इस तरह, वाराणसी, काशी और कन्नौज के बीच कई छोटे-छोटे गाँव उभरे, जो बिखरे हुए व्यापारिक केंद्र बन गए। ये छोटे व्यापारिक केंद्र धीरे-धीरे कस्बों में बदल गए, जो वाराणसी से गाज़ीपुर तक गंगा के किनारे फैले हुए थे।
खोई हुई काशी अब विद्वानों के लिए शोध का विषय बन गई है, और पुरातत्व प्रेमियों के लिए एक आकर्षक जिज्ञासा का केंद्र।
समय के साथ, इन विद्वानों के प्रयास सफल हुए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मृगदाव-सारनाथ की खोज थी, जो आंशिक रूप से उजागर हो चुकी है। लेकिन इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से आज भी खोज और अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं।
धूल और समय की परतों के नीचे अनगिनत मूल्यवान अवशेष छिपे हुए हैं, जो खोई हुई काशी के बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं।
प्राचीन काशी की पुनर्खोज कठिन हो गई है, क्योंकि इसका विनाश एक लंबे समय में, बार-बार होता रहा। जिस नगर को 1600 वर्षों (500 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक) में धीरे-धीरे लूटा और नष्ट किया गया, उसे दोबारा समझने और उजागर करने के लिए एक सतत, संगठित प्रयास की आवश्यकता होगी।
काशी की खोज अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है।
वाराणसी, जिसे आज भी एक जीवित नगर माना जाता है, की पुनर्खोज और भी कठिन हो गई है, क्योंकि हाल के समय में भी इसे बार-बार विनाश झेलना पड़ा है।
इन विनाशों के लिए अक्सर इस्लामी आक्रमणकारियों को दोष दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कारक, जिसने वाराणसी की मूल बनावट को पूरी तरह से मिटा दिया, वह था अंग्रेज़ी शासन।
अंग्रेजों के हाथों वाराणसी की बर्बादी इतनी निरंतर और अविवेकी थी कि वह प्राचीन वनभूमि, जो कभी ऋषियों, विद्वानों और साधकों का निवास स्थल थी, अंततः बिखर गई।
अधिकांश महत्वपूर्ण मंदिर और आश्रम अधिक सुरक्षित स्थानों की ओर खिसक गए। कई पूजनीय देवी-देवताओं की मूर्तियाँ, जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, गुप्त स्थानों पर छिपा दी गईं।
विशेश्वर (विश्वनाथ) मंदिर ने मूर्तिभंजकों का विशेष क्रोध आकर्षित किया। यह मंदिर नगर के सबसे ऊँचे स्थान पर स्थित था, और इसकी अपार संपत्ति लूट के लिए एक आसान लक्ष्य बन गई।
यह मंदिर बार-बार ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। विशेश्वर मंदिर विनाश की शक्तियों और श्रद्धालु भक्तों की जिद के बीच एक युद्धभूमि बन गया था।
इस मंदिर की अपनी एक अलग इतिहासगाथा है।
लगभग 1018 ईस्वी में, कन्नौज (कान्यकुब्ज), जो उस समय एशिया का सबसे समृद्ध और चमकदार नगर था, महमूद गज़नी की सेनाओं द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।
तब से लेकर, हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों की लूट और विध्वंस आक्रमणकारियों के लिए एक नियमित परंपरा बन गई। धर्म के नाम पर मंदिरों का विनाश उनके लिए संपत्ति, सत्ता और ज़मीन हथियाने का साधन बन गया।
यहाँ तक कि मठ और विद्यालय भी आक्रमणकारियों की धार्मिक उग्रता से अछूते नहीं रहे।
V
इन विनाशों का एक दुखद दुष्प्रभाव बलपूर्वक धर्मांतरण की समस्या थी।
शुरुआत में, धर्मांतरित लोग अपने पूर्व धर्म और समाज में लौटने की तीव्र इच्छा रखते थे। वे अपने रिश्तेदारों और मित्रों द्वारा फिर से अपनाए जाने की उम्मीद करते थे।
लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।
धर्मग्रंथों में सामान्यतः धर्मांतरण के खिलाफ सख्त आपत्तियाँ थीं। इसके अलावा, हिंदू समाज के सामने दो बड़ी बाधाएँ थीं — वे न तो मुसलमानों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर सकते थे, और न ही अपने धर्मांतरित भाइयों और रिश्तेदारों को वापस अपने धर्म में ला सकते थे, क्योंकि इस्लामी शरीयत के अनुसार ऐसा करने पर मौत की सजा का डर था।
कोई हिंदू किसी मुसलमान से विवाह भी नहीं कर सकता था, और ऐसे विवाह शरीयत कानून के अनुसार प्राणदंड के अधीन होते थे।
इन कठोर नियमों ने हिंदुओं के सामने लगभग कोई विकल्प नहीं छोड़ा। एक बार धर्मांतरित होने के बाद, लोगों को उसी धर्म में रहना पड़ता था।
अपने भाइयों के इस अन्यायपूर्ण तिरस्कार और अपने ही समाज द्वारा निर्दयी अस्वीकृति से आहत, धर्मांतरित लोग और अधिक कठोर बन गए। वे स्वयं मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विनाश में जुट गए। मंदिरों को तोड़ते हुए, वे असल में उस कठोर शुद्धतावादी सामाजिक ढाँचे को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे, जिसने उन्हें अस्वीकार कर दिया था।
यह वही लोग थे, जिन्हें उनके समाज ने, थोड़ी भी सहानुभूति के साथ, अपने बीच जगह दे सकती थी — भले ही कानूनों के दबाव में। लेकिन उन्हें वह सामुदायिक सहारा नहीं मिला, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी।
आज उपमहाद्वीप में जो सांप्रदायिक तनाव मौजूद है, उसकी जड़ें इसी भाई-भाई के बीच पनपी घृणा में हैं। बाद के विदेशी आक्रांताओं ने इस तनाव को केवल अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए हवा दी। लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि यह आत्मघाती प्रवृत्ति आज तक थमी नहीं है।
इस सामाजिक तनाव की झलक आज भी वाराणसी की जनसंख्या संरचना में देखी जा सकती है।
आज के वाराणसी में, प्राचीन पवित्र स्थलों के आस-पास — जहाँ कभी बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था — धर्मांतरित लोगों की बस्तियाँ आज भी संघर्षरत हैं। ये वे लोग थे, जिन्हें एक गर्वीले और कठोर समाज ने खारिज कर दिया था।
वे आज भी जैसे-तैसे अपने पूर्वजों के पारंपरिक व्यवसायों के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, जैसा वे प्राचीन काल में करते थे।
उनमें से अधिकांश कभी उन प्रसिद्ध उत्पादन समूहों से जुड़े थे, जिनके बारीक हस्तशिल्प चीन से रोम तक प्रसिद्ध थे।
अपने पूर्व भाइयों द्वारा अलग कर दिए जाने के बावजूद, वे आज भी अपनी पारंपरिक कलाओं में लगे हुए हैं। वे आज भी रेशम, कपास, पीतल, हाथीदांत, कांस्य, सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी, बेंत, घास और लाख से वस्तुएँ बनाते हैं।
यह तथ्य गौर करने लायक है कि अधिकांश हिंदू देवी-देवताओं की पत्थर और संगमरमर की मूर्तियाँ आज भी इन्हीं धर्मांतरित मुस्लिम शिल्पकारों के हाथों से बनती हैं।
अनादि काल से, काशी के व्यापारी और वाराणसी के कारीगरों ने मिलकर एक विशिष्ट सामाजिक संस्कृति का निर्माण किया है, जो धार्मिक निष्ठाओं में बदलाव के बावजूद अडिग बनी रही।
मंदिर की भूमि पर कब्जा करना, फिर वहाँ मुफ्त में रहने के लिए धीरे-धीरे मकान बनाना — ये बातें धर्मांतरण के बाद के लोगों के स्वतः अधिकार जैसे बन गए।
विजित, भयभीत हिंदू समाज ने, पराजय की निराशा में, न केवल मंदिरों से दूरी बना ली, बल्कि उनसे जुड़ी ज़मीनों के अधिकार भी छोड़ दिए।
उन्होंने उन खूबसूरत नक्काशीदार पत्थरों के लूट-मार पर भी विरोध करना छोड़ दिया, जिन्हें मंदिरों से निकालकर मस्जिदों और महलों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया गया।
फिर भी, धर्मांतरित कारीगर इन्हीं खाली पड़ी जगहों से चिपके रहे, जो बार-बार के आक्रमणों और सामाजिक पहचान के क्षरण के बाद खाली हो गई थीं।
इतिहास के इन मोड़ों और उतार-चढ़ावों ने लोगों के जीवन पर गहरे घाव छोड़े हैं।
विकल्पों की कमी के कारण, इन लोगों ने वहीं बस जाना चुना, जहाँ वे सुरक्षित रह सकते थे, और उन्होंने थोड़ा-बहुत जीवन-स्थान वहीं छीन लिया, जहाँ से उनके पूर्वज भाग खड़े हुए थे।
धार्मिक स्थलों को तोड़कर, उनके पत्थरों से नए भवन बनाना, पवित्र जलाशयों को भरकर वहाँ बस्तियाँ बनाना, अतिक्रमण करना, और खंडहरों पर अपनी दावेदारी जताना — ये सब धीरे-धीरे इन धर्मांतरित बस्तियों की लगभग परंपरा बन गईं।
वे टूटी हुई मंदिरों की ज़मीन को 'युद्ध में जीती हुई संपत्ति' मानते थे, और अक्सर पुराने दस्तावेज पेश करते थे, जिन पर उस समय के शासकों की मुहर लगी होती थी।
उनके कई दावे उन कागजात पर आधारित थे, जो उनके धर्मांतरित होने से पहले की ज़मीन-जायदाद के प्रमाण थे।
आज वाराणसी के अधिकांश मुसलमान वास्तव में उन संपत्तियों पर रहते हैं, जिन पर उनके पूर्वजों के पुश्तैनी अधिकार थे।
लेकिन इस तरह की अनियंत्रित तोड़-फोड़ और पुनर्निर्माण ने उन विद्वानों के लिए कई बाधाएँ खड़ी कर दी हैं, जो पुरानी वाराणसी और उसके धार्मिक परिवेश की खोज करना चाहते हैं।
इसके बावजूद, एक समुदाय के रूप में, वाराणसी के मुसलमानों ने अपने प्राचीन सामाजिक परिवेश के नैतिक मूल्यों को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया है।
वे अपनी इस्लामी एकता और अतिथि सत्कार को गर्व से दिखाते हैं, और अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों में जीते हैं।
यदि वाराणसी की किसी मुस्लिम बस्ती को गहराई से देखा जाए, तो एक सुखद सच्चाई सामने आती है — दोनों समुदाय एक-दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि वे अपने-अपने धार्मिक और सामाजिक नियमों की सीमाओं का पालन करते हुए भी, एक-दूसरे की रक्षा और सहायता के लिए खड़े रहते हैं।
विभिन्न समुदायों के प्रति सम्मान की यह परंपरा आज भी अवध (प्राचीन काशी-कोशल) की सामाजिक संस्कृति की एक बहुमूल्य विरासत है।
लखनऊ, रामपुर और जौनपुर के मुस्लिम शासकों ने भी इस सामाजिक समन्वय की भावना को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया।
VI
न तो बौद्ध, न मुसलमान, और न ही विदेशी विजेताओं की क्रूरताएँ — इनमें से कोई भी प्राचीन काशी के सामाजिक ताने-बाने को उतना क्षतिग्रस्त नहीं कर सका, जितना कि कुछ ही वर्षों के भीतर अंग्रेजों के अहंकारी और शासकीय रवैये ने कर दिया।
जीवन के लिए संघर्ष और एकता का जो भाव सदियों से वाराणसी में जीवित था, उसे अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन ने भीतर से खोखला कर दिया।
अपने द्वीप के संकीर्ण दायरे में सुरक्षित रहने वाले अंग्रेजों के लिए अहंकार और असहिष्णुता प्रशासन के नाम पर लूट का एक कारगर औजार बन गए।
उन्होंने भारत की संपत्तियों को बेशर्मी से लूटा, उसकी दौलत को समुद्र पार ले जाकर अपने समाज को समृद्ध बनाया। लेकिन उन्होंने यह सब इतने चतुराई से किया कि उनके कानूनी ढाँचे की आड़ में वे कभी भी किसी अदालत में दोषी सिद्ध नहीं हुए।
यह इतिहास में कानूनी डकैती का एक अनूठा उदाहरण है।
अंग्रेजी मानसिकता भारत जैसे विविधतापूर्ण महाद्वीप की संस्कृति को समझने, स्वीकारने या आत्मसात करने में पूरी तरह विफल रही।
वे इस बात को कभी नहीं समझ पाए कि एशिया — और विशेष रूप से भारत — में लोग कितनी विविधता के बावजूद मानव-आत्मा की एकता में जीते थे।
भारत उनके छोटे-छोटे षड्यंत्रों के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ।
और जब वे इसे नियंत्रित करने में असफल रहे, तो उन्होंने भारत के लोगों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने की योजना बनाई — जैसे भेड़ियों की तरह शिकार को फाड़कर धीरे-धीरे निगल लिया जाए।
उन्होंने यह सब किया, लेकिन कानून की आड़ में। कानून, जैसा कि कहा जाता है, कभी-कभी विवेकहीन भी हो सकता है।
एशिया — जो सभ्यता और संस्कृति की पृथ्वी पर सबसे पुरानी शरणस्थली थी — ने हमेशा सह-अस्तित्व और आपसी समझदारी की भावना के साथ जीना सीखा था।
लेकिन यह भावना अंग्रेजों की तीव्र विस्तारवादी महत्वाकांक्षा और धूर्त शोषण की भूख के लिए पूरी तरह से पराई थी।
अपनी सत्ता की भूख और पराजितों को अपमानित करने की जिद ने व्यापार के नाम पर आए इन व्यापारियों को जनता के मन से हमेशा के लिए दूर कर दिया।
जहाँ इस्लामी आक्रमणों ने वाराणसी को लालच और धार्मिक कट्टरता के चलते क्षति पहुँचाई, वहीं अंग्रेजों के शासन ने गहरी, अपमानजनक तिरस्कार की भावना से शहर की आत्मा को आहत किया।
वाणिज्य के नाम पर आए इन ज़मीनी समुद्री लुटेरों ने भारत पर स्थिर और न्यायसंगत शासन की आड़ में अपनी अनैतिक गतिविधियाँ जारी रखीं।
वे जिस स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात करते थे, वह केवल उनके द्वीप समाज के लिए थी।
भारत जैसे अंधकारमय एशियाई देशों के लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई।
वे अहंकार, अपमान और दिखावे के साथ जीते थे।
इतिहास के भयानक आक्रमणकारी — जैसे हूण, तैमूर, महमूद गज़नी, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली — भले ही रात के अंधेरे की तरह आए और नई सुबह के साथ चले गए।
लेकिन अंग्रेज — जिन्हें हैदर अली ने 'चूहे' कहा था — कभी खुद नहीं गए, जब तक कि उन्हें बलपूर्वक खदेड़ा नहीं गया।
जहाँ लखनऊ के इस्लामी शासकों ने अपने पीछे पड़ोसी प्रेम, कला और उदारता की परंपरा छोड़ी, वहीं ब्रिटिश शासकों ने भारत को सांप्रदायिक वैमनस्य, दंगे, और आपसी अविश्वास की दुखद विरासत दी।
भारतीय इतिहास ने ब्रिटिश शासन से पहले कभी सांप्रदायिक दंगों का अनुभव नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद, वाराणसी और उसकी मिश्रित संस्कृति आज भी सामाजिक शांति बनाए हुए है — उतनी ही शांत और स्थिर, जितनी गंगा की नीली धाराएँ।
यह शांति उतनी ही दृढ़ है, जितनी आनंदकानन के प्राचीन पर्वतीय आश्रमों की चट्टानें, जिन पर आज भी वाराणसी का शहर टिका हुआ है।
VII
1781 में, वाराणसी के शासक चेत सिंह के हाथों वॉरेन हेस्टिंग्स की हार ने उस श्वेत आक्रमणकारी को भड़का दिया, जो एक सच्चे नवधनाढ्य की तरह, एक प्राचीन राजवंश के उत्तराधिकारी के आचरण को समझने में पूरी तरह अक्षम था। जिस व्यक्ति को वह एक साधारण सामंती प्रमुख, एक मामूली देशी राजकुमार मानता था, उसके हाथों हारने से उसके अहंकार को गहरी ठेस पहुँची। अंग्रेजों की अजेयता का भ्रम एक साधारण देशी के हाथों चकनाचूर हो गया। कुछ गुमराह, निर्धन गद्दारों की मदद से उसने दूसरा प्रयास किया और अंततः सफल हुआ। हालाँकि वाराणसी को अपमानित और ध्वस्त कर दिया गया, फिर भी पिछली हार की चुभन हेस्टिंग्स को हमेशा सालती रही, और उसने शहर के साथ ऐसी निर्दयता से व्यवहार किया, जिसे आज के लोग शायद समझ भी नहीं सकते।
अंग्रेजों द्वारा वाराणसी का अंतिम विनाश उन 'विशेषज्ञ' विदेशी इंजीनियरों और नगर-निर्माताओं के माध्यम से किया गया, जिन्हें प्राचीन अवशेषों, इतिहास और एक पवित्र शिक्षा-स्थल के सम्मानित स्थलों को सँभालने की तनिक भी समझ नहीं थी। भारतीय पुरावशेष उनके लिए वेस्टमिंस्टर, वॉर्सेस्टर या टिंटर्न चर्चों के पत्थरों और स्लैब्स से कम मूल्यवान थे। जहाँ मुसलमानों के पास हिंदू परंपराओं की एक गहरी समझ थी (क्योंकि वे स्वयं कभी हिंदू ही थे, जो किसी और आस्था में परिवर्तित हो गए थे), वहीं इसके विपरीत, ईसाई शासकों को पवित्र स्मारकों, तीर्थ-स्नान स्थलों, शिक्षाकेंद्रों और वनाश्रमों के प्रति कोई सम्मान रखने का कारण ही नहीं दिखा।
शांत और मनोहर नदियाँ, जो कभी वाराणसी के प्रसिद्ध जंगलों के बीच से बहती थीं, जानबूझकर अवरुद्ध कर दी गईं और समतल कर दी गईं, ताकि यूरोपीय दर्शक आरामदायक पहिएदार गाड़ियों में, वर्दीधारी सुरक्षा के बीच नदी के किनारे 'सुरक्षित और आरामदायक' यात्रा कर सकें। नहीं, न बौद्ध कट्टरता, न मुस्लिम धर्मांधता, न तातारों और कुषाणों की हिंसा, न ही लुटेरों की निर्ममता — वाराणसी इन कारणों से नहीं, बल्कि अंग्रेज प्रशासन की सुनियोजित कुटिलता और अव्यवस्थित नगर-योजनाओं के कारण नष्ट हुई।
वाराणसी को ब्रिटेन के स्वार्थी, दूरदर्शिता से रहित साम्राज्यवादी एजेंटों ने नष्ट कर दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक पकड़ का प्रतिनिधित्व करते थे — विशेष रूप से वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, वैनसिटार्ट, बार्लो और इम्पी जैसे दंभपूर्ण एजेंटों ने। इनमें से वॉरेन हेस्टिंग्स का अहंकार इस बात से गहरा आहत हुआ था कि उसे 'सिर्फ' एक देशी राजकुमार, चेत सिंह ने परास्त कर दिया था।
यह साम्राज्यवादी तिरस्कार वाराणसी की आत्मा और उसकी विशिष्टता को धीरे-धीरे घुन की तरह खा गया। आज की वाराणसी, प्राचीन आनंदकानन की छाया तक नहीं है। पूरी चेतना एक दमनकारी, हृदयहीन विदेशी प्रशासन के नीचे दबकर टूट चुकी थी। यह पौराणिक नगर एक चिरस्थायी आघात से जूझ रहा था।
वास्तविक वाराणसी समाप्त हो चुकी थी। इसलिए उसकी पुनर्खोज की बात उठती है। इतिहास और संस्कृति के हर विद्यार्थी की यह नैतिक और नागरिक जिम्मेदारी है कि वह उस वाराणसी को देखने और महसूस करने की कोशिश करे, जो कभी थी — और अब नहीं है।
द्वीपवासियों के तथाकथित 'उदार शासन' ने वाराणसी के पवित्र वनाच्छादित पर्वतों की स्थलाकृति और परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। इन्हीं पहाड़ियों पर वैदिक-पूर्व काल का पवित्र रुद्रवास और आनंदकानन स्थित था — शिव और शैव संस्कृति का निवास।
यही वह वाराणसी थी, जिसकी महिमा का वर्णन काशीखंड, अग्नि पुराण, वायु पुराण, महाभारत, जातक कथाओं, ह्वेनसांग, फाहियान, अल-बरूनी और उन प्राचीन कवियों ने किया है, जिन्होंने इसके वैभव के गीत गाए। लेकिन वह रुद्रवास अब नहीं है। वह खोई हुई वाराणसी के मलबे के नीचे दब चुका है।
लगातार आक्रमणों और विनाशों से विवश होकर, रुद्रवास ने एक नए नाम — वाराणसी — के तहत शरण ली, जिसने आनंदकानन की शांति को किसी तरह बनाए रखने की कोशिश की। जैसे किसी शरणार्थी को अपना घर-बार गँवाने के बाद कहीं और शरण लेनी पड़ती है, वैसे ही काशी के बचे-खुचे लोग वाराणसी से चिपके रहे, जिसे शास्त्रों ने गृहस्थों के लिए 'वर्जित क्षेत्र' घोषित किया था।
आनंदकानन की जो अलौकिक शांति कभी इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, वह जल्द ही नष्ट हो गई, और एक संघर्षरत जनसमूह ने जो भी स्थान उपलब्ध था, उसे भर लिया। पूरा वरुणा-राजघाट क्षेत्र नगर में बदल गया, जो विश्वनाथ पहाड़ी और ज्ञानवापी की ढलानों तक फैल गया।
प्राचीन वाराणसी का चेहरा गहराई से बदलने लगा। आनंदकानन की आत्मा अपने भीतर के पतन से जूझने लगी।
राजनीतिक स्वार्थ, अज्ञानता और दार्शनिक उदासीनता के मिले-जुले कारणों से, आज के नगर-नियंताओं ने इन निरंतर विनाशों की ओर से आँखें मूँद ली हैं। वे न तो इस तोड़फोड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, न ही अतीत को बचाने और भविष्य को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता को समझते हैं।
वाराणसी — जो कभी पृथ्वी की सबसे पुरानी जीवित नगरी थी, जो अपनी शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा, आश्रमों, hermitages, साधना केंद्रों, विद्यालयों, अस्पतालों, तालाबों, झीलों, नदियों और चट्टानों के लिए प्रसिद्ध थी — आज भी अपमानित, लूटी और विकृत की जा रही है।
वाराणसी अब एक अति-भीड़भाड़ वाला बाज़ार बन चुकी है, जहाँ श्रद्धालुओं को सिर्फ इसलिए सहन किया जाता है, क्योंकि उनके पूजा-दान से बहने वाली पसीने की कमाई पर नगर के स्वार्थी लोग निर्भर हैं।
ऐसा लगता है जैसे नगर-नियंताओं ने वाराणसी को नीनवे, टायर, तक्षशिला और नालंदा की खोई हुई नगरी बनने के लिए छोड़ दिया है।
आधुनिक सुविधाओं के विस्तार ने वाराणसी की पहचान को और धूमिल कर दिया है।
आनंदकानन की वह पौराणिक शांति अब गायब है, और उसकी जगह अंधी रूढ़िवादिता और संकीर्ण लालच ने ले ली है।
प्राचीन वाराणसी का विशाल, फूला हुआ शरीर अभी भी समय के महासागर में तैर रहा है — अब पहचान में न आने लायक, लेकिन फिर भी अतीत के गौरव का एक अवशेष।
लेकिन इससे भी बड़ा दुख यह है कि वाराणसी की आत्मा बहुत पहले उड़ चुकी है, केवल एक खंडित, मृत देह को छोड़कर।
VIII
काशी सदियों पहले धूल में मिल गई थी। पुराने संस्कृत ग्रंथों में इन विनाशों का विस्तार से वर्णन भरा हुआ है। निकुंभ, क्षेमक, दिवोदास, प्रतर्दन I, प्रतर्दन II, अजातशत्रु, प्रसेनजित और अन्य शासकों के समय की लगातार मार के कारण, गणों और वैष्णवों, रुद्रियाओं और कापालिकों के लंबे संघर्षों के दबाव में, प्राचीन वाराणसी गहराई से आहत और विदीर्ण हो गई थी।
काशीखंड (K. Kh.) इन संघर्षों का स्पष्ट विवरण देता है, जिसे पारंपरिक इतिहास-ग्रंथों द्वारा भी पुष्टि मिलती है। जहाँ एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति पर, या एक धार्मिक विश्वास द्वारा दूसरे पर आक्रामकता के परिणामस्वरूप इन संघर्षों को देखा जा सकता है, वहीं ऐतिहासिक समय में ये झगड़े राजनीतिक युद्धों में बदल गए। ये लड़ाइयाँ आज भी अलग-अलग रूपों में जारी हैं।
भीष्म के काशीराज से युद्ध करने के समय से लेकर अजातशत्रु, प्रसेनजित, प्रतर्दन वंश, हैहय, सातवाहन और गहड़वालों के समय तक, काशी हमेशा भारतीय इतिहास के केंद्र में रही है।
इस्लामी आक्रमण तो बहुत बाद में हुए। वास्तव में, 1194 ईस्वी में शहाबुद्दीन गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन की सेनाओं के सामने काशी के जयपाल के आत्मसमर्पण के बाद ही, काशी की सुरक्षा विदेशी आक्रमणकारियों के लिए खुली।
जेम्स प्रिंसेप ने कुछ इस्लामी अभिलेखों का उल्लेख किया है, जिनमें संक्षेप में यह बताया गया है कि काशी पर बोनार नामक एक राजा शासन कर रहा था, जिसे 1117 ईस्वी में महमूद गज़नी ने पराजित किया था।
तब तक वाराणसी पहले ही अपनी स्थिति बदल चुकी थी, और काशी भी। प्राचीन काशी के सबसे पुराने स्मारकों में से केवल सारनाथ आज भी एक मौन साक्षी के रूप में खड़ा है।
3.सारनाथ
I
असल में सारनाथ को नष्ट किसने किया? क्या किसी एक कट्टर संप्रदाय ने एक बार में विनाश किया, या अलग-अलग समय पर कई संप्रदायों ने? यह एक अत्यंत विवादास्पद प्रश्न है। आज सारनाथ और उसके आसपास का क्षेत्र सुनसान खंडहरों में तब्दील हो चुका है। ये खंडहर हमें 500 ईसा पूर्व से लेकर बारहवीं शताब्दी के अंत तक के प्रमाण प्रदान करते हैं। 600 ईस्वी के आसपास ह्वेनसांग ने इसे पूर्ण अवस्था में देखा था। लिच्छवी वंश की राजकुमारी और वाराणसी के गहड़वाल राजा गोविंदचंद्र की रानी कुमारदेवी ने अपने उपहारों से इस स्थल को समृद्ध किया था।
तो फिर इस विनाश का कारण कौन बना? यह घटना निश्चित रूप से 600 ईस्वी के बाद हुई होगी और शायद इसके पीछे राजनीतिक कारण नहीं, बल्कि धार्मिक या सांस्कृतिक कारण रहे होंगे। क्या यह धार्मिक कट्टरता के कारण हुआ? लेकिन यह इस्लामी आक्रमण तो नहीं हो सकता था। तो फिर इस तबाही के लिए कौन ज़िम्मेदार था?
वैसे भी, यह विनाश एक दिन, एक वर्ष या कुछ वर्षों में नहीं हुआ। यह इस्लामी आक्रमणों से पहले ही शुरू हो चुका था। दरअसल, जब विदेशी आक्रमणों की भयंकर लहर आई, तब तक सारनाथ पहले ही एक भूतिया खंडहर में बदल चुका था, जहाँ की अफवाहों के अनुसार, रात में केवल राक्षस और दानव नृत्य करते थे।
संभावना है कि यह स्थान वज्रयान और पिशाच साधनाओं के विचित्र अनुयायियों से भर गया था, और साधारण ग्रामीण लोग इस पवित्र स्थल के चारों ओर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की कहानियों पर आसानी से विश्वास कर लेते थे।
इन भूत-प्रेत की कहानियों के बावजूद, दूर-दूर के ग्रामीण खंडहरों में बिखरी इमारतों की समृद्ध सामग्री को उठाने से नहीं चूके। इस सामग्री का उपयोग उन्होंने अपने घर बनाने के लिए किया। धनी लोग भी उन चौड़ी ईंटों, चमकदार पत्थरों और संग्रहणीय मूर्तियों को अपने भवनों को सजाने के लिए ले जाने से खुद को रोक नहीं सके।
विनाश की शुरुआत शायद दक्षिण के हैहयों और उत्तर के प्रतिहारों के बीच हुए निरंतर संघर्षों के दौरान हुई होगी। विद्वानों का मानना है कि रुद्रवास के भारशिव भी आंशिक रूप से सारनाथ के विनाश के लिए जिम्मेदार थे। उनके पास ऐसा करने का पर्याप्त कारण भी था।
उनकी अशिक्षित और अज्ञानी आँखों को वज्रयान की विकृत परंपराओं से घृणा हो सकती थी — जैसे पशुबलि, शराब का अनियंत्रित प्रयोग, पुरुषों और महिलाओं का अर्धनग्न या पूर्ण नग्न अवस्था में अनुष्ठान करना, शवों के साथ हस्तक्षेप, और संभावित मानव बलि। इन विकृतियों ने पवित्र विहारों को भी दूषित कर दिया था। यहाँ तक कि संघारामों (मठों और ननों के आश्रमों) के पवित्र परिसर भी नहीं बचे। ग्रामीणों को ये स्थान धोखे के जाल की तरह लगे, जहाँ उनके युवाओं और घरों को नष्ट किया जा रहा था। अज्ञान और आक्रोश से भरा एक क्रोधित समूह इस पवित्र विहार को जलाने और नष्ट करने के लिए पर्याप्त था।
इसी संदर्भ में, गहड़वाल वंश की शक्तिशाली शाही संरक्षक कुमारदेवी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी और संभवतः मंगोल मूल की महिला होने के नाते, वे स्वाभाविक रूप से तिब्बती वज्रयान के आकर्षण में बह गईं। इसने दिगंबर जैनियों के नग्न साधना पंथों की गिरावट को भी प्रोत्साहित किया।
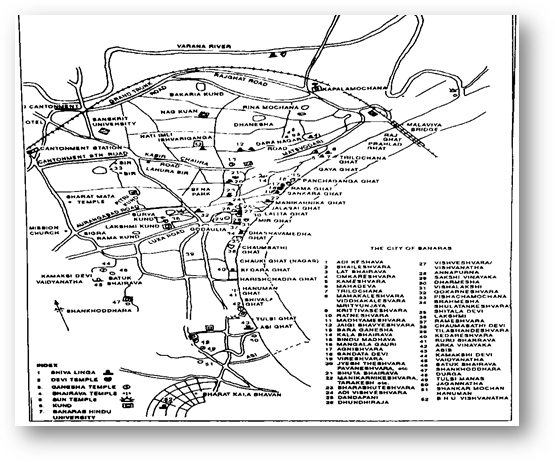
मानचित्र 3: वाराणसी मंदिरों को दर्शाता शहर
हालाँकि सुंग (187-30 ईसा पूर्व) और सातवाहन (30 ईसा पूर्व - तीसरी शताब्दी) ने सारनाथ की समृद्धि में योगदान दिया, लेकिन गहड़वालों ने भी — अपनी तांत्रिक रुचि के कारण — सारनाथ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वहाँ वैश्रवण, वज्रवाराही, मारीची, वसुंधरा जैसे तांत्रिक वज्रयान देवताओं की स्थापना की।
खुदाई में कुमारदेवी की ननों की मठ तक एक गुप्त भूमिगत मार्ग मिला है, जिसने इसकी रहस्यमय गतिविधियों के बारे में संदेह बढ़ा दिया। आर. डी. बनर्जी ने साहसपूर्वक सुझाव दिया कि यह मार्ग गुप्त साधना सत्रों के पुरुष प्रतिभागियों को गुप्त रूप से मठ तक पहुँचने की सुविधा देने के लिए बनाया गया था। स्वाभाविक रूप से अफवाहें फैलने लगीं, और लोगों के गुस्से का विस्फोट हुआ।
अमिताभ बुद्ध के महान युग की जगह अब भयावह तांत्रिक अनुष्ठानों ने ले ली थी। इससे वाराणसी के निवासियों की भावना को ठेस पहुँची, जो अब भी महान शिक्षक (शास्ता) की शिक्षाओं को पूजते थे। 1154 ईस्वी में राजा गोविंदचंद्र के शासन का अंत हुआ। उनके नियंत्रण के बिना, स्थितियाँ बद से बदतर हो गईं। तांत्रिक अनुष्ठानों की अफवाहों ने शैव संप्रदाय को क्रोधित कर दिया।
उन्होंने सारनाथ में तांत्रिक अनुष्ठानों के बराबर विशाल मंदिरों का निर्माण शुरू किया। जैतपुरा से मंडाकिनी तालाब तक, काशीखंड और तीर्थ विवेचनखंड में उल्लिखित कई प्रसिद्ध मंदिर इसी समय बने।
इन मंदिरों के माध्यम से, बुद्ध के प्रति सम्मान के बावजूद, वाराणसी के लोगों ने जनता का ध्यान विकृत तांत्रिक साधनाओं से हटाने की कोशिश की। अंततः, वीरशैवों का एक क्रोधित समूह ने सारनाथ के विकृत तांत्रिक विहारों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके साथ ही, सारनाथ के महान विहारों, मूर्तियों और सदियों से अर्जित प्रतिष्ठा का विनाश हो गया।
इसके बाद, जो बचा था, उसे महमूद गज़नी, गोरी, और अंततः जौनपुर के शर्की शासकों की सेनाओं ने नष्ट कर दिया। बारहवीं शताब्दी का सारनाथ एक वीरान जंगल में बदल गया, जो सात सौ वर्षों तक उपेक्षित पड़ा रहा।
अंततः, मृगदाव एक जंगल बन गया, और बुद्ध की विश्वप्रसिद्ध प्रतिमा मिट्टी और मलबे के नीचे दब गई — जिसे एक अंग्रेज़ आर्किटेक्ट ने खुदाई के बाद फिर से खोजा। यह कहना कठिन है कि सारनाथ का विनाश केवल विदेशी आक्रमणों के कारण हुआ। वाराणसी के निवासियों की धार्मिक असहिष्णुता और आंतरिक सामाजिक विघटन ने सारनाथ को लंबे समय तक अचेतना में धकेल दिया।
II
बौद्ध सारनाथ के विनाश के कारणों ने (जो वास्तव में ईसा पश्चात 100 तक काशी जनपद के भीतर स्थित था) आनंदकानन के रूप में विकसित होने में मदद की, जो आज की वाराणसी बनी, और इस नदी से घिरे आश्रम की सामाजिक-धार्मिक जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। यह क्रमिक परिवर्तन महाश्मशान से रुद्रवास, फिर गौरीपीठ, आनंदकानन, काशी, और अंततः वाराणसी तक हुआ। इस प्राचीन पर्वतीय निवास की यह सांस्कृतिक रूपांतरण प्रक्रिया इसके नामों में स्पष्ट रूप से झलकती है, जो अब तक इस प्राचीनतम नगर से जुड़े हुए हैं।
कालचुरी और प्रतिहारों के बीच निरंतर युद्धों ने काशी जनपद और सारनाथ दोनों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। फिर, 998 ईस्वी में, गहड़वालों ने इस पर अधिकार कर लिया।
बढ़ती जनसंख्या के दबाव में मूल वाराणस्या, जिसका अर्थ था 'वरुणा की ओर मुख वाला नगर', ने धीरे-धीरे अपना 'मुख' दक्षिण की ओर मोड़ लिया। नया नगर गंगा के किनारे दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। नगर का विस्तार इतना तीव्र और निर्णायक था कि शासकों ने इसकी सुरक्षा के लिए वरुणा के दक्षिणी तट पर एक किला बनाने का निर्णय लिया। इस नव-निर्मित किले ने गंगा-वरुणा संगम से नगर की रक्षा की। यह किला मत्स्योदरी से अधिक दूर नहीं था, जहाँ भारशिव (स्थानीय समुदाय) द्वारा निर्मित एक प्राचीन मिट्टी का किला अब भी कार्यरत था।
पुराने मिट्टी के किले की उपस्थिति, जो एक प्रसिद्ध नदी-किनारे के बाज़ार के पास थी, इस स्थान के महत्व को रेखांकित करती है। वहीं, गहड़वाल शासकों द्वारा संगम पर एक मजबूत किले का निर्माण इस महत्व को और भी पुष्ट करता है। व्यापारिक केंद्र और नगर की गतिविधियाँ उत्तर के सारनाथ क्षेत्र से हटकर दक्षिण में मांडाकिनी झीलों के आसपास बढ़ते नए नगर की ओर स्थानांतरित हो गईं।
गहड़वाल किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। विद्वानों का मानना है कि काशी के इतिहास के प्रामाणिक साक्ष्य अब भी रेलवे पुल के मार्गों और राजघाट थियोसोफिकल कॉलेज की नई इमारतों के नीचे दबे हो सकते हैं। जब 1905 में बनारस में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो राजघाट पठार, जहाँ अधिवेशन हुआ था, वहाँ विभिन्न प्रकार के बर्तनों और मिट्टी के टुकड़ों की भरमार मिली।
विद्वानों की इस धारणा को इस तथ्य से बल मिलता है कि पठार के पास आज भी एक उल्लेखनीय मस्जिद है, जो लगभग पूरी तरह से हिंदू संरचनाओं से लूटे गए सामग्रियों से बनी है। इस पठार के चारों ओर निर्माणों का यह संगम — (क) मिट्टी का किला, (ख) वरुणा और मच्छोदरी को जोड़ने वाली नहर, (ग) राजघाट किला, (घ) मस्जिद — इस तट के बढ़ते महत्व की ओर संकेत करता है। शहरी बस्तियाँ धीरे-धीरे आनंदकानन पर कब्जा कर रही थीं।
समर्पित पुरातत्वविदों ने तमाम चुनौतियों के बावजूद सराहनीय कार्य किया है। आज हम प्राचीन वाराणसी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका 60% हिस्सा इन विद्वानों की खोजों का परिणाम है। उन्होंने 14 विभिन्न परतों तक खुदाई की, और उनकी खोजों के परिणाम आज वाराणसी के भारत कला भवन में सुरक्षित हैं।
इस प्रकार, प्राचीन सारनाथ और उससे भी प्राचीन वाराणसी को आधुनिक स्मृतियों से पूरी तरह बाहर कर दिया गया; दोनों ही पहचान से परे गायब हो गए, और हम एक नए नगर को रुद्रवास और महाश्मशान की राख से उगते हुए देखते हैं।
सारनाथ के विनाश की अंतिम चोट मुस्लिम विजेताओं ने दी थी, लेकिन यह पूरी तरह से उनका कृत्य नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि सारनाथ की हत्या हुई थी, बल्कि ऐसा लगता है मानो यह एक बीमार बस्ती को हटा देने जैसा था।
ऐसे विनाश पूरे भारत में हो रहे थे: राजगृह, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन, उदयना, बल्लभी, कांची आदि। ये केंद्र, जो पहले ही आंतरिक संघर्षों से कमजोर हो चुके थे, बाहरी आक्रमणकारियों के लिए आसान लक्ष्य बन गए। हमें शिव, शक्ति, जैन, बौद्ध, और वैष्णव संप्रदायों के बीच चले कट्टर धार्मिक संघर्षों के प्रभाव को कमतर नहीं आँकना चाहिए। बोधगया आज भी इन धार्मिक संघर्षों की जीवित मिसाल है।
प्राचीन काशी के सबसे पुराने स्मारकों में से, केवल सारनाथ का धमेख स्तूप आज भी एक उदास प्रहरी की तरह खड़ा है। दूसरा प्रहरी, जो सारनाथ के रास्ते पर खड़ा है, एक लाल ईंटों की अष्टकोणीय संरचना है। यह एक टीले पर स्थित है, जिसकी ऊँचाई लगभग सत्तर फीट है। यह अकबर के शासनकाल में टोडरमल के पुत्र गोवर्धन द्वारा निर्मित एक मुगल संरचना है, जो हुमायूँ के शेरशाह के साथ युद्ध के दौरान एक दिन के ठहराव को स्मरणीय बनाती है।
जब कुषाणों ने पहली शताब्दी में काशी पर अधिकार कर लिया था, तब भी सारनाथ एक संपन्न जैन-बौद्ध केंद्र था। कनिष्क, जो बाद में बौद्ध अनुयायी बन गए, को काशी या मृगदाव सारनाथ को नुकसान पहुँचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस प्रकार का विनाश बंगाल के शशांक, शुंगों और कण्वों की ब्राह्मण शासित राजशाहियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया, जो खुद को हिंदू धर्म के रक्षक मानते थे और जैन-बौद्ध प्रभाव को मिटाने के लिए दृढ़ थे।
इन अंतर्धार्मिक संघर्षों की गूँज हमें काशीखंड में वर्णित गण-शिव और विष्णु युद्धों में सुनाई देती है। इस हिंदू पुनर्जागरण के प्रयासों के प्रमाण के रूप में, इस अवधि में अश्वमेध यज्ञ के लिए एक विचित्र दौड़ देखी जा सकती है। इसे खारवेल, समुद्रगुप्त, धृतराष्ट्र, गहड़वाल राजा गोविंदचंद्र, और पुष्यमित्र शुंग जैसे शासकों ने करवाया था।
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कुषाण विजय के समय तक, काशी हमेशा से एक प्रतिष्ठित हिंदू राज्य बना रहा। रुद्रवास, आनंदकानन, और वाराणसी को काशी के शासक एक पवित्र धरोहर मानते थे, जिसे उनके पूर्वजों और प्राचीन ब्राह्मणकालीन विधायकों ने सौंपा था।
बौद्ध केंद्रों का विनाश गोरी के समय तक लगभग पूरा हो चुका था। खिलजी, तुगलक और लोदी राजवंशों के लिए हिंदू-बौद्ध केंद्रों को बार-बार लूटना एक नियमित खेल बन चुका था। यह सिर्फ काशी की पवित्रता पर हमला नहीं था। खून केवल एक विचारधारा को नष्ट करने के लिए नहीं बहाया जाता। इसके पीछे एक भौतिक कारण भी था — धन, संपत्ति और सत्ता। धन ही शक्ति है। शक्ति को नष्ट करने के लिए धन का हस्तांतरण आवश्यक था।
लेकिन असल वाराणसी, जो काशी की आत्मा थी, वह आज के नगर के उसी हिस्से में स्थित थी, जो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच फैली हुई है। इसे ओंकारखंड और विश्वेश्वरखंड के नाम से जाना जाता था। आक्रमणकारियों ने सारनाथ या प्राचीन काशी को पूरी तरह खत्म नहीं किया; वे केवल मंदिरों की दौलत लूटने आए थे, क्योंकि उनके सैनिकों को वेतन नहीं मिलता था — वे लूट के हिस्से पर निर्भर थे। इसलिए ये विनाश इतने तीव्र और निर्णायक थे।
III
स्किथियन युग के बाद, और वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रभाव के तहत, गणों और द्रविड़ों की सहायता से जगह-जगह मंदिर और मंदिर परिसरों का निर्माण शुरू हुआ। जहाँ पहले केवल कच्चे शिवलिंग, असंगठित गणेश प्रतिमाएँ, और "बीर" के ठूंठ पाए जाते थे, वहीं कुषाण और तांत्रिक प्रभाव के चलते पहली शताब्दी ईस्वी तक अत्यंत कलात्मक मूर्तिकला का विकास हुआ। यह प्रवृत्ति, (जैसे कि पाणिनि, चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, कल्हण और अश्वघोष के ग्रंथों में वर्णित है) भारत की संस्कृति के लिए उत्तर-पश्चिमी हिंदूकुश और गांधार क्षेत्र से आया एक बहुमूल्य उपहार थी, जब तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने शिखर पर था। उस समय के भारत के कठोर आर्य समाज ने अभी तक मूर्तियों, मूर्तिपूजा और देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को अपनाया नहीं था।
आज हम जिन मंदिरों को देखते हैं, वे मूल इंडो-वैदिक संस्कृति का हिस्सा नहीं लगते। आनंद कुमारस्वामी और हाइनरिख़ ज़िमर के अनुसार, मंदिर वास्तुकला भारत में मेसोपोटामिया और ईरानी सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव के तहत विकसित हुई। इसने मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के साम्राज्यवादी प्रभाव को मजबूत किया। मंदिर, मंदिर की मूर्तियाँ, मंदिर अनुष्ठान और मंदिर संगठन, ये सभी पश्चिम एशिया की परंपराओं से प्रभावित प्रतीत होते हैं, जो केवल मैसेडोनियन आक्रमण और पार्थियन उपनिवेशीकरण के बाद भारत में आए।
मंदिरों से जुड़े अनुष्ठान ब्राह्मणवादी विस्तारवाद के अधीन होते गए। मंदिर की औपचारिकताओं की कठोरता, वर्ग-विशेषाधिकार, और अनुशासन की सख्ती ने पूरे धार्मिक तंत्र को जकड़ लिया। ईरानी-बेबिलोनियन आर्यों ने धीरे-धीरे मंदिर अनुष्ठानों को जटिल बना दिया, जहाँ भक्तों से केवल भूमि, आभूषण और फसलों का दान ही नहीं, बल्कि युवा कन्याओं को भी देवताओं के मनोरंजन के लिए समर्पित करने की माँग की गई। पुजारियों ने यह अनुशंसा की, और जनता ने इसे स्वीकार कर लिया। प्रत्येक मंदिर लुटेरों, डाकुओं और वासना में डूबे आक्रमणकारियों के लिए एक अत्यंत आकर्षक लक्ष्य बन गया।
वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की विस्तृत अनुष्ठानिक परंपराओं ने नई ऊँचाइयों को छुआ। जहाँ रुद्रवास में केवल अग्निकुंड, नदी और कुंडों में जल, और कुछ शिवलिंग, नागदेवता, गणदेवता या बीर ही थे, वहीं गुप्तकाल के बाद की वाराणसी में भव्य स्थापत्य और मूर्तिकला की श्रृंखला ने जगह बना ली। इस काल की भारतीय मूर्तिकला और कांस्य प्रतिमाएँ मानव सभ्यता की उत्कृष्ट उपलब्धियाँ थीं।
वर्ष के प्रत्येक दिन को किसी न किसी विशेष प्रार्थना के लिए चिह्नित किया गया। प्रत्येक विशेष दिन मंदिर की तिजोरी में नए चढ़ावे जोड़ता रहा। वैदिक यज्ञ की परंपरा धीरे-धीरे समाप्त हो गई, और उसका स्थान अनवरत उपवास, पर्व, स्नान, दान, और विभिन्न देवी-देवताओं की रात्रि-जागरण सहित अनगिनत प्रार्थना-परंपराओं ने ले लिया। भक्ति की इस अर्थव्यवस्था ने एक पुजारी-वर्ग को जन्म दिया, और मंदिर संस्कृति ने एक शक्तिशाली समूह को जन्म दिया, जिसके अपने निहित स्वार्थ थे। वैदिक धर्म धीरे-धीरे पृष्ठभूमि में चला गया।
बौद्ध स्तूप और चैत्य, भव्य रूप से निर्मित प्रभावशाली मंदिरों के लिए रास्ता छोड़ने लगे, जिनमें अधिकांश में बड़े-बड़े स्नान कुंड थे, जिनकी पक्की सीढ़ियाँ पानी तक जाती थीं। काशी महात्म्य, काशीखंड, महाभारत, और तीर्थ विवेचनखंड एक स्वर में इन मंदिरों, उनकी प्रतिमाओं, और कुंडों के जल की "चमत्कारी शक्ति" की महिमा का गुणगान करते हैं।
यह याद रखना आवश्यक है कि इस्लामी विनाश की अधिकांश कहानियाँ मुख्य रूप से तीर्थ केंद्र वाराणसी से संबंधित हैं, सारनाथ से नहीं। वर्षों में पवित्र वनस्थली एक भीड़भाड़ वाला और व्यस्त शहर बन गई थी। प्रारंभिक मुगल काल (अकबर को छोड़कर) और बाद के मुगल शासकों के समय में राजपूत और मराठों ने हिंदू धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर वाराणसी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने घाटों का निर्माण किया, कई मंदिर बनाए, और पवित्र कुंडों की मरम्मत की। इनमें से, विश्वेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रयासों की विशेष चर्चा की जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, काशी नगरी या वाराणसी नगरी भारत के सबसे आकर्षक शहरों में से एक बन गई, और यह प्रतिष्ठा आज भी बरकरार है।
हालाँकि, इस विकास में एक गहरी त्रासदी छिपी थी। पुराना आनंदकानन, रुद्रवास, जिसे शिव अत्यंत प्रिय मानते थे, और जिसे मानव हस्तक्षेप से बचाकर रखा गया था, वह शहरीकरण की व्यावसायिक लालसा के दाँतों में पिसने लगा। पर्यावरणीय आपदा ने पुराने आनंदकानन को निगल लिया।
मानवीय प्रगति एक खतरनाक दानव की तरह साबित हुई। जैसे-जैसे जंगल, झीलें, पहाड़ियाँ और नदियाँ गायब होती गईं, वैसे-वैसे मंदिरों को सोना, चाँदी, रत्न, रेशम, हाथी दाँत और विभिन्न सजावटी वस्तुओं से लाद दिया गया। देश भर से चुनी हुई सर्वोत्तम कन्याओं को एकत्र किया गया और देवी-देवताओं के दिव्य आनंद के लिए समर्पित किया गया। यह राहत की बात थी कि हिंदू अनुष्ठानों में केवल कन्याओं को अर्पित किया जाता था, न कि बालकों को, जैसा कि प्राचीन ओरिएंटल मंदिरों में प्रचलित था।
जहाँ प्राचीन आनंदकानन-रुद्रवास-गौरीपीठा अपनी वनों, कुंडों, नदियों और उपवनों के लिए प्रसिद्ध थी, वहीं नया शहर मंदिरों, महलों, आनंद उद्यानों और बाज़ारों से भरा हुआ था, जो एक पुनर्जीवित हिंदू एकता का प्रतीक बन गया।
पुजारी और ब्राह्मण इस नई सामाजिक संरचना में सबसे प्रभावशाली वर्ग बन गए, क्योंकि उन्होंने लगभग पूरी तरह से कला, विज्ञान और दर्शन के सैद्धांतिक अध्ययन और अनुसंधान को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा शहर विदेशी यात्रियों और विद्वानों जैसे अल-बिरूनी, इब्न बतूता, फिच, बर्नियर और टवर्नियर की प्रशंसा का केंद्र बन गया।
IV
मंदिर ने एक और उपेक्षित सत्य को उजागर किया। वैदिक देवता तो लुप्त हो गए, लेकिन वैदिक लोग किसी तरह जीवित रहे, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से उस देशी जनसंख्या के साथ घुल-मिल गए, जिसे उन्होंने पहले के समय में तिरस्कृत कर दिया था और यज्ञ स्थलों से दूर रखा था। (देखें: मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के नियम)।
इंद्र, वरुण, प्रजापति, अर्यमन, अग्नि, नासत्य, यम, अश्विन जैसे वैदिक देवताओं के लिए कभी मंदिर नहीं बने, लेकिन गणदेवता, भैरव, देवियाँ और शिवलिंगों के साथ उनके पशु साथी के लिए कई मंदिर बनाए गए। जब यह सब हो रहा था, वैदिक देवता मानो इन बदलावों से एक सुरक्षित और सतर्क दूरी बनाए रखने का निर्णय कर चुके थे।
इस प्रकार की दैवीय अवधारणाओं में हुए इस रूपांतरण ने विद्वानों को महायान और हड़प्पा के उन देवताओं की याद दिलाई, जिन्हें वैदिक ब्राह्मणवाद के दिनों में समान रूप से नकार दिया गया था।
ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था, जिन्हें कभी बौद्ध धर्म ने हटाया था, धीरे-धीरे फिर से लोकप्रिय मान्यता और भक्तों की श्रद्धा प्राप्त करने लगे। चैत्य मंदिरों की जगह भव्य हिंदू मंदिरों ने ले ली, और तीर्थंकर और बोधिसत्वों की जगह हिंदू अवतारों ने ग्रहण कर लिया। ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता के तमाम चतुर दावों के बावजूद, आर्य परंपरा की एक पतली परत ही बची रह गई थी, जो अब तेजी से क्षीण होते हुए वैदिक प्रभाव को ढँकने की कोशिश कर रही थी।
तंत्र ग्रंथों के विस्तृत अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान हिंदू ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों की परंपरा पर तंत्र-महायान दर्शन और विधियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। वर्तमान हिंदू अनुष्ठानिक स्वरूप वास्तव में तंत्र, महायान, वज्रयान, और प्राचीन प्राक-द्रविड़ और द्रविड़ जनजातीय परंपराओं का मिला-जुला परिणाम है, जो कभी देशज पूजा के मूल स्वरूप थे। हवन का स्थान पूजन ने ले लिया।
इस संदर्भ में संत औखरिय वैखानस का महत्वपूर्ण योगदान याद आता है, जिनका औखरियसूत्र (ईसा पूर्व काल) वैदिक यज्ञ परंपरा के लगभग विलुप्त होने के बाद के वैष्णव अनुष्ठानिक पूजा के लिए आधार बना।
V
इसलिए, हमें यहाँ प्राचीन हिंदू अवशेषों के निशान मिलने पर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता। सारनाथ में स्थित शिवलिंग, जिसे सारंगेश्वर के नाम से जाना जाता है, और उसका मंदिर, जिसकी वास्तुकला इस क्षेत्र के सामान्य मंदिरों की शैली और रूप से भिन्न है, हमें ताम्रलिप्ति के वर्गाभीमा मंदिर की याद दिलाता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह मंदिर वज्रयोगिनी महायान परंपरा से जुड़ा हुआ था।
लोकप्रिय मान्यता के अनुसार, यह सारंगनाथ लिंग और सौराष्ट्र का सोमनाथ लिंग एक ही काल के थे। काशी महात्म्य में एक लिंग, सांगेश्वर का उल्लेख है, जिसे सारंगेश्वर या सारंगेश्वर के नाम से जाना गया है।
सारनाथ परिसर में मौजूद यह टीला और मंदिर, जो आज भी सक्रिय हैं, अत्यंत प्राचीन प्रतीत होते हैं। वर्तमान में मंदिर के सामने का तालाब कभी एक विशाल झील हुआ करता था (3000 x 1000 फीट) और इसे नरोकरा (ना-क्रोध या अक्रोध) या सारंगताल कहा जाता था। इसके पास एक छोटी झील थी, जो अब बंद हो चुकी है, जिसे नयाताल कहा जाता था, जिसका अर्थ है ‘बाद की झील’। इस क्षेत्र का एक गाँव वराही के नाम से जाना जाता था, और एक पड़ोसी गाँव अब भी गुरनपुर या गुरुपुर के नाम से जाना जाता है, जो उस समय के तांत्रिक गुरुओं के प्रभाव को दर्शाता है। सारनाथ के खंडहर आज भी जीवित इतिहास की धड़कन की तरह प्रतीत होते हैं।
1921-23 की उन निश्चिंत, सुनहरी बालपन की बरसातों में, लेखक ने कितनी ही बार सारनाथ के हरे-भरे क्षेत्र में घूमते हुए पके हुए मीठे अंजीर और ताजे सिंघाड़े खाए। विनम्र बौद्ध भिक्षु एक संस्कृत बड़बड़ाने वाले अजीब लड़के को कितनी सहजता से अपनाते थे। दोपहर की मधुमक्खियों से भरी लंबी दोपहरें कुमारदेवी की रहस्यमयी ननों के मठों और भिक्षुओं के निवासों की भूमिगत सुरंगों की खोज में बीत जाती थीं। पीपल, रीठा, नीम, और इमली के पेड़ तालाब के किनारे की शांति बनाए रखते, जबकि मोरों की अचानक तेज पुकार सांपों की उपस्थिति की चेतावनी देती थी।
अब वह पूरा दुनिया जैसा रोमांटिक दृश्य, मेहनती गाँव की लड़कियाँ और उनके साथी, सब कुछ एक अमीर शहरीकरण के नीचे ढँक दिया गया है, जो केवल क्षणिक पर्यटकों और विद्वानों के लिए एक सजावटी स्वागत प्रस्तुत करता है।
कुल मिलाकर, सारनाथ, जो कभी वाराणसी के निकट एक महत्वपूर्ण केंद्र था, कालचुरी-हैहय संघर्षों के बाद धीरे-धीरे वीरान हो गया। यह क्षेत्र इतिहास से पूरी तरह मिट गया, जब तक कि 1815 में कर्नल मैकेंजी ने इसे दोबारा खोजा नहीं। लगभग 1500 वर्षों तक विनाश की ताकतें यहां बेरोकटोक अपना खेल खेलती रहीं।
1815 के बाद ही यह खंडहर प्रकाश में आए, जब मैकेंजी ने देखा कि अमूल्य स्थापत्य सामग्री और सजावटी पत्थरों को अमीर और गरीब दोनों ही बिना किसी रोक-टोक के अपने निर्माण कार्यों के लिए उठा रहे थे। उन्होंने इस लूट को रोकने का संकल्प लिया। उन्होंने पाया कि जगत सिंह, जो काशी के राजा चेत सिंह के सचिव थे, स्वयं व्यक्तिगत उपयोग के लिए बहुमूल्य सामग्री उठा रहे थे। इसके बाद, जैतपुरा, सिगरोल और अलईपुरा के मुस्लिम निवासी भी बरकरारिकुंडा और पितृकुंडा जैसे प्रसिद्ध मंदिरों से सामग्री उठाने लगे, जिन्हें काशीखंड में उनकी स्थापत्य और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए सराहा गया है। दुर्भाग्यवश, इन दोनों स्थलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, क्योंकि कोई कनिंघम, ओर्टेल, मैकेंजी या मार्शल इस बर्बरता के खिलाफ खड़े नहीं हुए।
इन पवित्र स्थलों पर हुए इन विध्वंसों के लिए केवल बाहरी आक्रमणकारी या अविश्वासी ही जिम्मेदार नहीं थे। इन प्राचीन धार्मिक अवशेषों पर हिंसा करने वाले कई बार स्वयं हिंदू या धर्मांतरित हिंदू थे। कई मामलों में खंडहरों में उनके अपने अतीत की परछाइयाँ झलकती थीं। लालच न तो जाति देखता है, न धर्म।
1851 में, मेजर किट्टो ने बनारस के ऐतिहासिक क्वीन्स कॉलेज की गॉथिक संरचना के निर्माण के लिए सारनाथ से पत्थर, मूर्तियाँ और अन्य सजावटी वस्तुएँ लीं। उन्होंने एक पूरा अशोक स्तंभ उठाकर कॉलेज के खेल मैदान के किनारे लगा दिया। उन्होंने एक संग्रहालय भी बनवाया, जहाँ उन्होंने बचे हुए टुकड़ों को संरक्षित किया। (कम से कम उस व्यक्ति में मूल्य की समझ तो थी, भले ही संवेदनशीलता की नहीं।)
सारनाथ लगातार अपमानित होता रहा।
जब एक ओर सारनाथ अपनी ऐतिहासिक महिमा के कारण खोजकर्ताओं, गृह-निर्माताओं और कला-चोरों को आकर्षित करता रहा, तो दूसरी ओर सरल ग्रामीण, जो इन अवशेषों के मूल्य से अनजान थे, लेकिन प्रशासनिक शक्तियों को दूर रखना चाहते थे, उन्होंने वहाँ की ज़मीन के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ गढ़ लीं — कि वहाँ भूत, प्रेत, आत्माएँ और कब्रों पर नृत्य करने वाले राक्षस रहते हैं।
वे कहते थे कि वहाँ की ज़मीन से ईंटें खुद उगती हैं। जितनी ईंटें उठाओ, उतनी और निकल आती हैं। इस चतुराई ने 700 वर्षों तक शोधकर्ताओं को दूर रखा। विशाल खंडहरों के बीच केवल एक स्तूप, एक मंदिर, एक बड़ा तालाब और कुछ छोटे तालाब, जहाँ सिंघाड़े उगते थे, बचे रहे।
सारनाथ से लेकर मार्कंडेय क्षेत्र तक पूरे इलाक़े में हर जगह टीले, टूटी हुई दीवारें, और अधखुले स्थान बिखरे हुए थे, जो सदियों से अमीर और गरीब ग्रामीणों के लिए निर्माण सामग्री के असीमित स्रोत बने हुए थे।
VI
पुरानी काशी समाप्त हो चुकी थी। सारनाथ, जो वर्तमान वाराणसी से केवल 16 मील की दूरी पर स्थित है, अब वर्तमान शहर के दक्षिण में है। पुराना शहर और उसके उपनगर उत्तर-पूर्व की ओर फैले हुए थे; चौखंडी, भीतरी, कैथी, मार्कंडेय, सोदेपुर, संभवतः वर्तमान गाजीपुर तक।
जब ह्वेन त्सांग वाराणसी आए, तो उन्होंने सारनाथ और विश्वनाथ मंदिर दोनों का दौरा किया। उन्होंने कई मंदिर देखे। इससे पता चलता है कि दोनों शहरों के बीच की भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाजन धीरे-धीरे धुंधला हो रहा था।
उनके समय में वाराणसी के बाजारों में सोना, चांदी, रेशम, हाथीदांत और हस्तशिल्प जैसे कीमती सामानों की भरमार थी। बाद में, अल-बरूनी (1030 ईस्वी) आए, लेकिन उनके अभिलेख वाराणसी की शैक्षिक और आध्यात्मिक संपदा पर अधिक जोर देते हैं।
गंगा और वरुणा के संगम से लेकर गंगा और गोमती के संगम तक, यह पूरा क्षेत्र काशी-कोसला राज्य का हिस्सा था, जैसा कि महाकाव्यों में वर्णित है। जैन और जातक ग्रंथों के अनुसार, यह शहर लगभग 900 वर्ग मील (लगभग आधुनिक दिल्ली के क्षेत्रफल के बराबर) में फैला हुआ था। यह विशाल क्षेत्र वर्तमान वाराणसी में समा पाना असंभव लगता है, जब तक कि यह भीतरी और सोदेपुर तक नहीं फैला हो।
ह्वेन त्सांग द्वारा वर्णित विश्वनाथ मंदिर वास्तव में कृतिवासेश्वर भी हो सकता है। विश्वनाथ हमेशा लिंग रूप में पूजे जाते रहे हैं, लेकिन जो मूर्ति ह्वेन त्सांग ने देखी, वह ठोस तांबे (कांस्य) की बनी हुई थी और 100 फीट ऊंची थी। यह केवल वरुणा नदी के पास स्थित किसी मंदिर की मूर्ति हो सकती है, क्योंकि वह वाराणसी के उत्तर से प्रवेश कर रहे थे।
एक प्राचीन और विस्तृत शहर के पतन के बाद, यह स्वाभाविक था कि निकटवर्ती आनंदकानन धीरे-धीरे लोगों से भरने लगे। शरणार्थी पहाड़ियों के इधर-उधर बसने लगे। पेड़ों को काट दिया गया, और उत्तर-दक्षिण की गलियां जैसे कि बिसेसरगंज से असि-लंका या कालभैरव, चौखंभा, कचौड़ी गली, बंगाली टोला, पीतांबरपुरा, और शिवाला सांप की तरह फैलने लगीं।
शहर दो भागों में बंट गया। एक काशी, जो राजघाट के किले के आसपास विकसित हुई, जहां प्राचीन गहड़वाल वंश के राजा रहते थे। पुराना किला आज भी खड़ा है, जैसे एक मूक गायक, जो बीते हुए वैभव और गिरी हुई प्राचीरों की कहानियां सुनाता है। 'राजघाट' नाम आज भी उस शाही निवास की निकटता की याद दिलाता है, जो वरुणा नदी और वर्तमान रेलवे पुल के पास था।
दूर उत्तर में एक बाहरी शहर विकसित हुआ — गाजीपुर, जिसे भीतरी, कैथी और सोदेपुर ने पंख दिए। पुरानी काशी, जैसा कि पुराणों और बौद्ध काल के ग्रंथों में वर्णित है, संभवतः इसी क्षेत्र के बीच में स्थित रही होगी। जनसंख्या के घनत्व और महत्व के कारण, गाजीपुर और सोदेपुर का विस्तार नदी के पार हुआ, जिससे एक और नया शहर — बक्सर — विकसित हुआ। इन दोनों इस्लामिक नामों की उपस्थिति प्राचीन काशी-कोसला के महत्व को दर्शाती है।
इस प्रकार, काशी और सारनाथ धीरे-धीरे वाराणसी के साथ विलीन हो गए। पुराना शहर और मठ एक धुंधली स्मृति बनकर रह गए। उसी तरह आनंदकानन का वनाच्छादित आश्रम भी यादों में खो गया।
यादें खंडहरों से प्रेम करती हैं। इन खंडहरों की खोज पहली बार 1815 में कर्नल मैकेंजी ने की थी, लेकिन वह प्रहरी, जो इस समृद्ध स्थल का संकेत देता था, महान धमेक स्तूप था, जिसे सम्राट अशोक (269-232 ईसा पूर्व) की उदारता से खड़ा किया गया था। इसे समय-समय पर राजाओं के दान से संरक्षित और समृद्ध किया गया था।
इनमें अंतिम और रहस्यमयी योगदान गहड़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र की पत्नी लिच्छवी कुमारदेवी का था। हमें उनकी याद उनके मठ, उस गुप्त सुरंग के लिए आती है, जो मठ तक जाती थी, और उनके रात्रिकालीन वराही की उपासना के लिए, जिसकी प्रतिमा आज भी सारनाथ संग्रहालय की शोभा बढ़ाती है।
4.मणि-नामित वाराणसी
I
अब समय आ गया है कि वाराणसी से जुड़े नामों की श्रृंखला को उसकी वास्तविक सांस्कृतिक दृष्टि में देखा जाए। जातक कथाओं में उल्लिखित काशी के कई काव्यात्मक नामों के अलावा, कुछ नाम ऐसे हैं जो उस पहाड़ी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, जो नदी की अर्धचंद्राकार मोड़ को घेरती है और जिसके ऊपर आज की वाराणसी का भव्य दृश्य आलोकित होता है।
ये नाम हैं — महाश्मशान, रुद्रवास, आनंदकानन, गौरीपीठ, अविमुक्त, वाराणसी और काशी।
इनमें से पहले पांच नाम आज भी प्रचलित हैं, जिसका श्रेय वाराणसी के पारंपरिक पुजारी समुदाय को जाता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान इन नामों का जाप करते हैं ताकि श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक लाभ मिल सके। इस तकनीक के माध्यम से, उन्होंने शहर के सांस्कृतिक क्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी को जीवित रखा है। इन नामों में प्राचीन शहर की सांस्कृतिक रूपांतरण की पूरी कथा निहित है।
महाश्मशान
प्राचीन काल में, जब ये पहाड़ियां आदिम निवासियों द्वारा बसी हुई थीं, उनके अर्ध-घुमंतू जीवन के कारण इस क्षेत्र को महाश्मशान कहा गया, यानी एक विशाल दाह संस्कार क्षेत्र। वर्तमान हरिश्चंद्र घाट से लेकर आदि केशव घाट तक, संपूर्ण नदी तट एक विशाल श्मशान के रूप में प्रयुक्त होता था।
आज का मणिकर्णिका घाट, जो दाह संस्कार के लिए प्रसिद्ध है, वास्तव में अपेक्षाकृत आधुनिक स्थल है। एक राजकीय अधिकारी और एक अंत्येष्टि कर्मी के बीच हुए विवाद के कारण, एक प्राचीन और पवित्र स्नान स्थल को श्मशान भूमि में परिवर्तित कर दिया गया।
'महाश्मशान' में 'महा' शब्द केवल आध्यात्मिक उच्चता का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसका अर्थ था विशाल क्षेत्र, जहां लोग अपने प्रियजनों का दाह संस्कार करते थे, या जहां साधक आत्मा की मुक्ति के लिए तपस्या करते थे।
इस क्षेत्र में गृहस्थों को बसने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह क्षेत्र विशेष रूप से संन्यासियों और साधकों के लिए आरक्षित था। यही कारण है कि प्राचीन काल में वाराणसी का शहरी भाग वरुणा नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ था, और शहर भीतरी और सोदेपुर तक फैला हुआ था। सारनाथ भी काशी के निकट स्थित था।
रुद्रवास
गौतम बुद्ध के उपदेशों का एक बड़ा भाग निरग्रंथ और दिगंबर साधुओं के विरुद्ध था। ये साधु, जो अक्सर नग्न या भस्म-लिप्त होते थे, अपनी साधना के लिए इन पहाड़ियों को उपयुक्त मानते थे।
समय के साथ, रुद्र के अनुयायी, जैसे गणा, किरात, पिशाच, नाग, राक्षस और सिद्ध, इन पहाड़ियों को अपना आश्रय स्थल बनाने लगे। वे सभी गैर-वैदिक समुदायों से संबंधित थे। इन समुदायों की उपस्थिति के कारण इस स्थान को 'रुद्रवास' कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है 'रुद्र का निवास'।
आनंदकानन
पुराणों में वर्णन है कि इस क्षेत्र को विशेष रूप से माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए चुना गया था। उन्होंने इस स्थल को इसलिए पसंद किया क्योंकि यह वनों से आच्छादित, शांत और देवताओं की भव्यता से दूर एक निजी आनंद स्थल था।
इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र आर्यों के प्रभाव से अछूता था, और यहां सदा एकांत और शांति का वातावरण बना रहता था। इसी कारण इस क्षेत्र को 'आनंदकानन' कहा गया — आनंद का उपवन।
गौरीपीठ
जब शिव ने अपने गणा के साथ इस क्षेत्र को अपना निवास बनाया, और माता गौरी ने इसे स्थायी रूप से अपनाने का निर्णय लिया, तो यह स्थान 'गौरीपीठ' कहलाया।
इस नाम ने इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण तांत्रिक पीठ के रूप में प्रतिष्ठित किया, जहां शिव और शक्ति की संयुक्त साधना की जाती थी। यह क्षेत्र धीरे-धीरे तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र बन गया।
अविमुक्त
सदियों के आध्यात्मिक अनुभवों से यह विश्वास प्रबल हुआ कि वाराणसी शिव और शक्ति की अविच्छिन्न उपस्थिति का केंद्र है। इस विश्वास के कारण इसे 'अविमुक्त' कहा गया, यानी ऐसा स्थान जहां दिव्य युगल कभी अलग नहीं होते।
वाराणसी
'वाराणसी' नाम की व्युत्पत्ति को लेकर कई मत हैं। सबसे प्रसिद्ध व्याख्या यह है कि यह नाम वरुणा और असि नदियों के नामों से बना है। हालांकि, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नाम 'वरुणा के सम्मुख स्थित' शहर से आया है।
काशी
'काशी' नाम मूल रूप से एक जनपद का नाम था, न कि किसी एक शहर का। जातक कथाओं में इस नगर को हमेशा 'वाराणसी' कहा गया है, न कि काशी।
इस प्रकार, काल के थपेड़ों और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बावजूद, वाराणसी ने अपने प्राचीन नामों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक विरासत को आज तक जीवित रखा है। हर नाम, हर कथा, इस अमर शहर की अद्वितीयता की गवाही देता है।
II
ऐसी कथाओं की लोकप्रियता और वहां रहने वाले अनूठे आध्यात्मिक साधकों के कारण, इस क्षेत्र को 'रुद्र लोगों का घर' कहा जाने लगा, जो एक प्राचीन आर्यपूर्व जनजाति थी। उमा-महेश्वर पंथ के साथ मिलकर, इन दो धाराओं ने उन लोगों की आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा किया।
वैदिक लोग अभी तक इस रहस्यमयी, सुंदर, और नदी किनारे फैले हुए जंगल के बारे में पूरी तरह अनजान थे, जो आमतौर पर अंतिम संस्कारों के लिए उपयोग किया जाता था। समय-समय पर, विभिन्न आर्य राजकुमारों के नेतृत्व में, वैदिकों ने रुद्रवास से रुद्रियाओं और गाना (भारा) शिवों को हटाने और इस आकर्षक स्थान पर कब्जा करने का प्रयास किया।
अब तक, वे समझ चुके थे कि विष्णु, सूर्य, प्रचेता, यम और अग्नि जैसे देवताओं के स्थायी मंदिर बनाना, और वाजपेय, अश्वमेध, अग्निष्टोम, सौत्रमणि जैसे बड़े यज्ञ आयोजित करना, अधिक स्थायित्व और उद्देश्यपूर्णता लाएगा। दशाश्वमेध घाट इसी सोच का एक स्मारक है।
पुराण और मिथकीय संदर्भ इन संघर्षों की गूंज से भरे पड़े हैं, जो गहड़वालों (1090) के समय तक अनवरत जारी रहे। इन प्राचीन धार्मिक संघर्षों के अंत में, एक अर्ध-राजनीतिक समझौते के माध्यम से सह-अस्तित्व स्थापित हुआ, जिसने वैदिकों को स्थानीय गणों को वाराणसी में शांति बनाए रखने के लिए अंतिम प्राधिकारी के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया।
युद्ध से थके हुए वैदिकों ने महसूस किया कि इस भूमि के लाभों को साझा करने का एकमात्र तरीका स्थानीय लोगों के अधिकारों को मान्यता देना और उनका सम्मान करना था। इस सह-अस्तित्व के लाभों को साझा करने के लिए, दो स्थायी 'रक्षक' नियुक्त किए गए। इन दो गैर-आर्य यक्ष-रक्षकों का नेतृत्व स्वयं यक्षों के स्वामी कुबेर ने किया, जिन्हें गणेश या विनायक के रूप में जाना जाने लगा, अर्थात् एक नियुक्त 'मार्गदर्शक' जो स्थानीय शांति के प्रभारी थे (मत्स्य पुराण)।
पूरी पहाड़ी स्थल और सीमाएं गण-देवताओं के मंदिरों से घिरी हुई थीं। इस शांति के एकमात्र गारंटर के रूप में, यक्ष-नेता कुबेर, गणपति के रूप में, गणों के स्वामी, ने इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली (शतपथ ब्राह्मण; मत्स्य पुराण)। उनके साथ, दो और प्रकार के रक्षक माने गए: एक भैरव, और दूसरे 'बीर'। बीर के अपने लट-आकार के प्रतीक चिन्ह होते थे, जो मोटे, छोटे खंभे के रूप में होते थे, जिन्हें सिंदूर (पारा ऑक्साइड) से ढका जाता था, और रेशमी कपड़े और फूलों की माला से सजाया जाता था।
आज भी वाराणसी के अंदर और बाहरी किलेबंदी में फैले इन भैरवों, बीरों और गणपतियों के कई मंदिर चुपचाप उन सतत संघर्षों की गवाही देते हैं, जो इस भूमि पर अंतिम कब्जे के लिए दो ऐतिहासिक नस्लों के बीच लड़े गए थे।
इतिहास और पुराण दोनों ही इन संघर्षों की कहानी बताते हैं। इन लड़ाइयों के निशान संभवतः चार से अधिक पीढ़ियों तक चले युद्धों को दर्शाते हैं — हैहय, परमार, विटहव्य, हर्यश्व, दिवोदास, और आलर्क। इन युद्धों को केवल परी कथाओं के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाण पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं हैं।
इसी तरह के युद्ध यक्ष हरिकेस और पूर्णभद्र के बीच भी हुए थे। मुद्दा शिव थे, जिनकी भक्ति हरिकेसा करते थे। उनके साथी उनकी शैव परंपरा से नाराज थे, और इस तरह यक्ष और शैवों के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध वर्षों तक चला, जब तक कि स्वयं शिव के लोगों (भारा-शिव) ने हस्तक्षेप नहीं किया। हरिकेसा को काशी का मुख्य रक्षक बनाया गया, और उनके दो साथी उद्भ्रम और संभ्रम शिव मंदिर के द्वारपाल बने (मत्स्य पुराण)। आज भी, वाराणसी के केदारनाथ मंदिर के भीतर इन दोनों की प्रभावशाली प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं।
राक्षस क्षेमक और हैहयों के बीच की लड़ाइयां (भद्रसेन्य या आलर्क, काशी खंड) राक्षस संस्कृति के अंत के साथ समाप्त हुईं, और दिवोदास के पोते आलर्क ने काशी को राक्षस प्रभाव से मुक्त कराया। (राक्षस एक शक्तिशाली जाति थी, न कि ब्राह्मणीय पुराणों में वर्णित 'आदमखोर'। यक्ष और राक्षस एक दूसरे के निकट संबंधी थे।)
इस यक्ष-राक्ष संस्कृति से शिव संस्कृति में यह परिवर्तन, रुद्रवास को आनंदकानन में बदलने की प्रक्रिया थी।
हमें इसे सिर्फ मिथक मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। इतिहास इन पुराणीय कथाओं की पुष्टि करता है। पुराण अपने समय के अनुरूप, काव्यात्मक शैली में ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन क्योंकि ये घटनाएं अलंकारिक भाषा में व्यक्त की गई हैं, हम उन्हें पूरी तरह नकार नहीं सकते। हमें अनाज के साथ भूसे को उड़ा देने की बजाय, इतिहास के सच को खोजने का प्रयास करना चाहिए।
गुप्त काल के अंत तक, वाराणसी विभिन्न धार्मिक संघर्षों में उलझी रही। जैन और बौद्ध धर्म के साथ-साथ, प्राचीन तांत्रिक समुदाय (बाद में बौद्ध हीनयान-यक्ष अनुष्ठानों के अनुयायी) दो विशिष्ट संप्रदायों में बंट गए — शैव और शक्त। स्किथियन, ग्रीक और फारसी प्रभावों से आई नई धार्मिक धारणाओं ने वाराणसी के तांत्रिक समाज में नित नई उपासनाओं को जन्म दिया। ये सभी वाराणसी में एक स्थान के लिए संघर्षरत थे, जो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था।
इस प्रकार, पुराणीय कथाओं में वर्णित ये संघर्ष महज कवियों की कल्पना नहीं थे, बल्कि इतिहास की वास्तविकता को पकड़ने का एक काव्यात्मक प्रयास थे।
III
छठी से तेरहवीं शताब्दी के बीच वाराणसी पर एक ब्राह्मणवादी वंश, गहड़वालों का शासन था। उनके संरक्षण में वाराणसी एक ब्राह्मणवादी गढ़ बन गई। इसी काल में वाराणसी की अधिकांश पुरातात्विक खोजें, मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेष उभरकर सामने आए। इस समय तक समस्त हिंदू भारत ने वाराणसी को हिंदू धर्म के सर्वोच्च केंद्र के रूप में मान्यता दी। विद्वान और छात्र वाराणसी में एकत्र होते थे। पुराणों की रचना हो रही थी, और महान मीमांसा आचार्यों द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रंथ लिखे जा रहे थे।
गहड़वालों के शासन के एक सदी बाद, चीनी यात्री विद्वान फाहियान और ह्वेन त्सांग ने वाराणसी का चरम वैभव वर्णित किया। समय के साथ अन्य यात्रियों ने भी इस धार्मिक नगरी का वर्णन किया। तेरहवीं शताब्दी तक वाराणसी की हिंदू संसार में सर्वोच्चता निर्विवाद हो गई।
इस काल के लिए एक सबसे विश्वसनीय स्रोत एक शिलालेख है, जिसे एक यात्री 'पंथ' ने छोड़ा था। इस शिलालेख में भवानी, या चंडी की मूर्ति की स्थापना का वर्णन है। इस देवी का उनका वर्णन स्पष्ट रूप से उनके शक्ति की वीर-साधना की ओर झुकाव को दर्शाता है। यह शिलालेख वाराणसी में प्राचीन तांत्रिक परंपरा के उदय का सबसे ठोस प्रमाण है। आठवीं शताब्दी तक तांत्रिक परंपराएं वाराणसी में पूरी तरह स्थापित हो चुकी थीं। यह इस बात का पक्का संकेत है कि वज्रयान ने महास्मशान, गौरीपीठ के निवासियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। 'पंथ' चाहे जो भी रहे हों, वे चंडी, चामुंडा के उपासक थे, जो तंत्र परंपरा की विशिष्ट देवी थीं, जिन्हें श्मशान, बलि का रक्त और मानव अवशेष प्रिय थे।
ग्यारहवीं शताब्दी में गहड़वाल वंश का शासन स्थापित हुआ। सौ वर्षों से अधिक समय तक, उनके शासन में वाराणसी ने महान ऊंचाइयों को छुआ। शहर मंदिरों, तीर्थयात्रियों, बाजारों, यात्रियों, छात्रों, विद्वानों, और निपुण सुंदरियों से भरा हुआ था।
हम पंथ शिलालेख से उद्धृत करते हैं: "उस समय की वाराणसी धर्म, अर्थ और काम के तीनों लोकों का समाहार थी।" दूसरे शब्दों में, यह शिलालेख पुष्टि करता है कि वाराणसी न केवल धार्मिक रूप से महान थी, बल्कि एक व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी संपन्न थी। 'अच्छा समय बिताने' के लिए भी यह शहर अद्वितीय था। "श्रद्धालु यहाँ जीने और मरने आते थे; शिव कभी अपने प्रिय स्थल को नहीं छोड़ते थे... सड़कें चौड़ी और भीड़-भाड़ वाली थीं... ऊंचे मंदिरों के शिखर और सुंदर महिलाएं समान रूप से शहर की शोभा बढ़ाते थे। वाराणसी का तीर्थ इतना प्रभावी था कि वह सभी पापों को नष्ट कर सकता था, यहां तक कि ब्रह्महत्या जैसे महापाप को भी।"
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दृश्य से लुप्त हो चुके थे, लेकिन तंत्र जीवित रहा, जैसा कि आज भी जीवित है।
वाराणसी और संपूर्ण हिंदू संसार के बारे में हमें गहड़वाल राजा गोविंदचंद्र के दरबार के प्रधान पंडित लक्ष्मीधर की एक विश्वकोशीय रचना से जानकारी मिलती है। उनकी पुस्तक 'कृत्य कल्पतरु' में सभी संभावित हिंदू अनुष्ठानों पर सैकड़ों निबंध शामिल हैं, और यह चौदह खंडों में लिखी गई है। लेकिन उनके एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ 'तीर्थ विवेचनखंड' (1150) का भी उल्लेख आवश्यक है, जिसमें वाराणसी के 550 स्थापित हिंदू तीर्थों का वर्णन है।
IV
अधिकांश मंदिरों के अवशेष अब खोज पाना कठिन है, क्योंकि इस्लामी आक्रमणों के बाद अंग्रेजों के 'शहर बसाने' के उत्साह ने इन प्राचीन स्थलों को मिटा दिया। फिर भी, जो मंदिर आज भी बचे हैं, वे यह संकेत देते हैं कि ये मंदिर प्राचीन बस्ती की सीमाओं के साथ व्यवस्थित रूप से फैले हुए थे। आज के शहर के केंद्र में मौजूद कुछ मंदिर, जैसे देवरिया-बीर या खोजवा, हमें यह नहीं भूलने देना चाहिए कि दो हजार साल पहले यह क्षेत्र केवल एक उपनगरीय जंगल था। भोजू-बीर, लौरिया-बीर जैसी बस्तियां इसकी गवाही देती हैं।
यह भी साबित करता है कि प्राचीन वाराणसी की मुख्य बस्ती ओंकारखंड से आगे नहीं फैली थी। ओंकारखंड से लेकर विश्वनाथखंड तक का विस्तार धीरे-धीरे हुआ लगता है।
ओंकारखंड की सीमा के साथ आज भी कई गणेश मंदिर मिलते हैं, जो अभी भी 'जीवित' हैं और नियमित रूप से पूजे जाते हैं। ये मंदिर हैं:
सृष्टि विनायक, साक्षी विनायक, कोना विनायक, देहली विनायक, चिंतामणि विनायक, गोप्रेक्षा विनायक, हस्ती विनायक, सिंदूर विनायक, धुंडी विनायक, अर्घ्य विनायक, डंडेश्वर विनायक, दुर्गा विनायक, भीमचंड विनायक, उद्दंड विनायक, पाशपाणि विनायक, खर्व विनायक, और सिद्धि विनायक।
यदि हम वर्तमान शहर के असि छोर से वरुणा छोर तक यात्रा करें और पंचकोशी क्षेत्र की सीमाओं के चारों ओर एक चक्र या चाप खींचें, तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन सीमाओं को कितनी सावधानी से संरक्षित किया गया था। असि के पास अर्क विनायक है, और पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हुए उत्तर में वरुणा तक आते-आते ये विनायक मंदिर एक के बाद एक मिलते हैं, जो आठ दिशाओं को घेरते हैं:
(1) अर्क विनायक, (2) दुर्गा विनायक, (3) भीमचंड विनायक, (4) देहली विनायक, (5) उद्दंड विनायक, (6) पाशपाणि विनायक, (7) खर्व विनायक, (8) सिद्धि विनायक।
इसके अलावा, एक आंतरिक चक्र भी था, जो अंतरगृह या विश्वनाथखंड की आंतरिक पवित्रता की रक्षा करता था। इस आंतरिक चक्र की रक्षा करने वाले गणपति मंदिर थे: धुंडी विनायक, साक्षी विनायक, महाराजा (डंठहस्त) विनायक (बड़ा गणेश), और मोड़ा विनायक।
इसी तरह, गणदेवताओं के मंदिर भी आज तक मौजूद हैं, जो हमें वाराणसी के यक्ष-वंशीय अतीत की याद दिलाते हैं। इनमें प्रमुख हैं: शूलपाणि, मुद्गरपाणि, विनायक, कुस्मांडा, गजतुंड, जयंत, मदोत्कट आदि।
(संभावना है कि गणदेवताओं के नाम मूल रूप से गणभाषा में रहे होंगे, क्योंकि गण संस्कृत नहीं बोलते थे। बाद में ये नाम संस्कृत में बदल दिए गए और आज उसी रूप में प्रचलित हैं। लेकिन इससे हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।)
इन गणदेवताओं के साथ-साथ, हमें काशी के भैरव मंदिरों की उपस्थिति भी ध्यान में रखनी चाहिए। ये 64 हैं, जिनके साथ 64 योगिनियां भी जुड़ी हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण आठ भैरव हैं: कपालि, असितांग, रुरु, चंड, क्रोधन, उन्मत्त, भीषण, और संहार।
जहां यक्षों और नागों की पूजा प्राचीन पूर्व-आर्य संस्कृति की उपस्थिति को दर्शाती है, वहीं एक और संस्कृति भारत में प्रवेश कर चुकी थी — सूर्य की पूजा। सूर्य की पूजा का चलन संभवतः मिस्र और ईरान से आया था। अपोलो, मिहिरा, या गवस्ति की पूजा वैदिक नहीं थी, खासकर उनके मंदिर से जुड़े अनुष्ठानों में। वैदिक धर्मग्रंथों में सूर्य पूजा का मंदिर-आधारित स्वरूप नहीं मिलता।
लेकिन ग्रीक, कुषाण और शकों के प्रभाव से यह परंपरा भारत में जड़ें जमा चुकी थी। वाराणसी में हमें बारह सूर्य मंदिर मिलते हैं, जो इस परंपरा के बने रहने का प्रमाण हैं। स्थानीय निवासी आज भी इन मंदिरों में नियमित दर्शन करते हैं, खासकर मार्गशीर्ष और माघ महीनों में।
इन बारह सूर्य मंदिरों के स्थान इस प्रकार हैं:
1. लोलार्क (भदैनी, असि के पास)
2. उत्तरार्क (बकरिया कुंड)
3. संबलादित्य (सूर्य कुंड)
4. द्रौपदादित्य (वर्तमान विश्वनाथ मंदिर के पश्चिम में)
5. मयूखादित्य (मंगला गौरी)
6. खाखोल्कादित्य (कामेश्वर)
7. अरुणादित्य (त्रिलोचना)
8. वृद्धादित्य (मीर घाट)
9. केशवादित्य (आदिकेशव)
10. गंधादित्य (ललिता घाट)
11. यमादित्य (बीरेश्वर मंदिर)
12. विमलादित्य (गोधौलिया, गोदावरी के पास)
अब तक हमें यह समझ में आ गया है कि वाराणसी की प्रमुख सांस्कृतिक पहचान हमेशा एक गैर-वैदिक, शिव-प्रधान संस्कृति रही है, जो वैदिक रूढ़िवादिता को चुनौती देती रही है। वाराणसी कभी भी शुद्ध वैदिक नहीं रही, न ही कभी होगी। यह स्थान आज भी एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है, जहां वैदिक सिद्धांतों को स्थानीय परंपराओं के साथ मिलाकर एक अनूठा और संतुलित धार्मिक अनुभव बनाया जाता है।
दूसरे शब्दों में, रुद्रियाओं और शुद्ध वैदिकों के बीच सदियों तक चली लड़ाई के बाद, वैदिक संस्कृति को समाहित कर वर्तमान हिंदू संस्कृति को गढ़ने की प्रक्रिया को वाराणसी ने सबसे बड़ा समर्थन दिया।
इसलिए, वाराणसी को हिंदू धर्म का महान केंद्र माना जाता है। वास्तव में, यहीं पर हिंदू धर्म को परखा, परिष्कृत और नया स्वरूप दिया गया। वाराणसी का आध्यात्मिक स्वरूप आज भी उदार, समावेशी और जीवन से भरपूर है। रूढ़िवादी इसे शास्त्र-विरोधी मान सकते हैं, लेकिन सच्चे आध्यात्मिक साधकों के लिए यह अब भी मुक्ति की शरणस्थली है। काशी का स्थान आज भी आध्यात्मिक मुक्ति की साधना के केंद्र के रूप में सर्वोच्च है।
V
वाराणसी में तांत्रिक परंपरा के विकास ने यहाँ की सांस्कृतिक संरचना और जीवनशैली को अत्यधिक प्रभावित किया है, जिसके प्रभावों को आसानी से पहचाना या सराहा नहीं जाता। 'अविमुक्त' शब्द अपने भीतर एक गहरी तांत्रिक ध्वनि समेटे हुए है, जिसे समझने के लिए वाराणसी के रहस्यमय स्वरूप की गहराई में उतरना होगा।
पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 'आनंदकानन' और 'गौरिपीठम' जैसे नामों में छिपे हुए रहस्यमयी अर्थ होते हैं, जिन्हें सामान्य व्यक्ति या अप्रशिक्षित साधक आसानी से नहीं समझ सकते। ये नाम वाराणसी की आध्यात्मिक विशिष्टता को इंगित करते हैं।
वाराणसी की पहाड़ियों और आसपास की घाटियों को शास्त्रीय संदर्भों में तीन खंडों में विभाजित किया गया है: केदारखंड, विश्वनाथखंड, और ओंकारखंड। ये तीनों खंड एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, जिसमें पहाड़ियाँ और उनसे जुड़ी घाटियाँ शामिल हैं।
प्राचीन काल में, इन तीनों खंडों को सामूहिक रूप से 'रुद्रवास' कहा जाता था। उस समय यह क्षेत्र घने जंगलों और झीलों से आच्छादित था, इसलिए इसे 'कानन' (उद्यान) कहा जाता था। इस स्थान को 'आनंद' (आनंद) क्यों कहा गया, इसका विवरण पहले ही दिया जा चुका है। लेकिन अब हमें ठहरकर, विचार करके, और तांत्रिक रहस्यों की गहराई में जाकर 'अविमुक्त' नाम की गूढ़ तांत्रिक महत्ता को समझना होगा।
पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों में काशी-कोसला की भौगोलिक और राजनीतिक सीमा स्पष्ट की गई है। इसका विस्तार गंडकी और गोमती नदियों के बीच बताया गया है, जबकि दक्षिण की ओर इसकी सीमा गंगा द्वारा निर्धारित होती है। जातकों के अनुसार, यह जनपद लगभग 300 योजन (2400 वर्ग मील) में फैला हुआ था। प्राचीन इतिहासकार अल्तेकर के अनुसार, काशी जनपद का विस्तार आधुनिक कानपुर से बलिया तक था, जिसमें मिर्जापुर, टांडा, चुनार, विंध्याचल, भदोही, गाजीपुर और सोदेपुर शामिल थे।
इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नदी, 'बंगंगा', गंगा की एक उपधारा थी, जो आगे चलकर 'मृतक गंगा' के नाम से जानी गई। यह धारा अब सूख चुकी है, लेकिन इसकी निशानियाँ आज भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। पुराणों में वर्णित 'मृतक गंगा' की उपस्थिति काशी की भौगोलिक महत्ता को और भी गहराई से समझने में मदद करती है।
पुराणों में वाराणसी को हमेशा एक नगर के रूप में वर्णित किया गया है। आज भी वरुणा नदी के किनारे एक प्राचीन मिट्टी की बाँधनुमा संरचना देखी जा सकती है, जिसे मानसून के दौरान गंगा की बाढ़ से शहर की रक्षा के लिए बनाया गया था। यह संरचना आज भी जैतपुरा, नाटे इमली, आदमपुरा, जगतगंज और चौकाघाट के आसपास बाढ़ से बचाव करती है। ‘घाट’ शब्द स्पष्ट रूप से नदी के किनारे ठहरने के स्थान को दर्शाता है।
यह संरचना दर्शाती है कि वाराणसी एक सुव्यवस्थित नगर था, जिसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। यह न केवल इस शहर की भौगोलिक महत्ता को रेखांकित करता है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक निरंतरता को भी दर्शाता है, जो तांत्रिक परंपराओं और रहस्यमय साधना पद्धतियों से गहराई से जुड़ी हुई है।
VI
बुद्ध का इसिपत्तनम् इस क्षेत्र को शामिल करता है, जिसमें उत्तरी आनंदकानन भी सम्मिलित है। किसी भी स्थिति में, वाराणसी और इसिपत्तनम् के बीच एक सूक्ष्म अंतर था। इसिपत्तनम् का नाम ऋषियों या 'पवित्र पुरुषों' की बसावट को दर्शाता है।
बौद्ध ख्याति वाला सारनाथ इसिपत्तनम् के पड़ोस में था, जो एक वन्य आश्रम था, और वहाँ के जंगलों में जानवर निडरता से घूमते थे, जिससे इसे एक और वर्णनात्मक नाम मिला, मृगदाव (जहाँ जानवर घूमते हैं)। सारनाथ निश्चित रूप से आज की तरह सूना और वीरान नहीं था, बल्कि मृगदाव से लेकर वरुणा नदी के किनारे तक का क्षेत्र अच्छी तरह बसा हुआ था।
जनसंख्या केवल निरंतर हमलों के खतरे के कारण स्थानांतरित हुई, जब तक कि गहड़वाल शासकों के समय में, उनकी बुद्धिमत्ता ने नगर को स्थानांतरित करने, एक किले और पुल का निर्माण करने, और कई स्थानों को विकसित करने का निर्णय नहीं लिया। चौका घाट उन स्थानों में से एक था।
आज जिसे हम सारनाथ के रूप में जानते हैं, वह संभवतः इसिपत्तनम् का उत्तरी छोर रहा होगा। बुद्ध के समय, वर्तमान 'बाज़ार' क्षेत्र आज की तरह नहीं था। एक समय, बुद्ध ने स्वयं भैरवों के कठोर मार्ग को अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे त्याग दिया। उन्होंने आत्म-संवर्धन के लिए पूर्ण एकांत की विकृत विचारधारा को छोड़ दिया। उन्हें समाज की आवश्यकता थी, जैसे समाज को उनकी आवश्यकता थी।
बाद में उन्होंने मृगदाव में अपने पंचवर्गीय शिष्यों को उपदेश दिया कि क्यों उन्होंने कठोर मार्ग छोड़ दिया। मृगदाव निश्चित रूप से वर्तमान सारनाथ के चारों ओर का वन क्षेत्र था, जिसमें आंशिक रूप से वह क्षेत्र भी शामिल था, जो अब कनिंघम उत्खनन के अंतर्गत है। सात से आठ सौ वर्षों तक, महान स्तूप के आसपास के विहारों को उत्तर और दक्षिण के विभिन्न शाही घरानों से उदार अनुदान प्राप्त होते रहे। यह विश्वास करना असंभव है कि महान विहार क्षेत्र में साधारण मानव बस्तियाँ नहीं रही होंगी, जो उत्तर में वरुणा नदी के किनारे तक फैली हुई थीं।
सारनाथ का आश्रम वास्तव में मृगदाव के पास स्थित था। लेकिन इसिपत्तनम्? यह स्थान वरुणा के करीब रहा होगा और दोनों तटों पर फैला हुआ होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी तटों से लेकर वास्तविक मृगदाव-सारनाथ तक, नदी के किनारे की भूमि, स्तूप क्षेत्र की सीमा तक, अच्छी तरह से व्यवस्थित बागों और विभिन्न प्रकार के पेड़ों से आच्छादित थी, और महान श्रेष्ठियों (व्यापारियों) ने इस क्षेत्र में अपने विश्राम गृह और उद्यान बनाए थे। इस क्षेत्र में बड़े उद्यान और विश्राम गृह बनाने की परंपरा आज भी बनी हुई है।
वैसे भी, यह क्षेत्र, जो आज इतना वीरान और उजाड़ दिखता है, कभी एक लोकप्रिय नगर के विस्तार का हिस्सा रहा होगा, जो एक शहरी व्यापारिक समुदाय द्वारा बसा हुआ था, जो मुख्यतः नदी व्यापार पर निर्भर था, जहाँ वरुणा उनकी मुख्य 'राजमार्ग' थी। किसी प्रकार की विपत्ति, जैसे निरंतर अराजकता या युद्ध का खतरा, लोगों को दक्षिणी तट पर जाने के लिए मजबूर कर सकता था, जहाँ उन्हें शाही संरक्षण प्राप्त था।
वाराणसी को हमेशा एक नगर के रूप में संदर्भित किया गया है। यह भी दर्शाता है कि जहाँ मृगदाव एक उद्यान स्थल प्रदान करता था, वहीं इसिपत्तनम् पूरी तरह से आश्रमों से बना हुआ था। दोनों के बीच यह सूक्ष्म अंतर, विशेष रूप से सारनाथ के नष्ट होने के बाद (पहले (क) ब्राह्मणीय क्रोध द्वारा, और बाद में (ख) इस्लामी आक्रमणों (1018) द्वारा पूरी तरह से जमीन पर समतल कर दिया गया था) धुंधला हो सकता था। जो इस्लाम नहीं कर पाया, वह स्थानीय लुटेरों ने लंबे समय तक की लूट के माध्यम से पूरा कर दिया।
नगर वाराणसी, जिसे वारणस्या (वरुणा + अस्य = वह नगर जो वरुणा की ओर मुख करता है) के रूप में भी जाना जाता था, एक लोकप्रिय व्यापार केंद्र था, जो नदी के दोनों तटों पर फैला हुआ था।
वाराणसी शब्द की व्याख्या वरुणा और असी शब्दों की मदद से करना शायद काव्यात्मक छूट का परिणाम रहा होगा। यह काव्यात्मक हो सकता है; फिर भी, यह आखिरी व्याख्या कल्पना में बस गई है, जैसा कि कविता करती है। हम इस संदर्भ में कुछ अन्य काव्यात्मक नामों का उल्लेख करते हैं, जिन्हें समय-समय पर वाराणसी पर आरोपित किया गया है: सुदर्शन, सुरंधन, ब्रह्मवर्धन, पुष्पवती, राम (या रम्या) और मालिनी या मुकुलिनी। जनपद का नाम काशिपुर था, जिसकी राजधानी पोटली थी (इसका नाम विभिन्न जातकों में मिलता है)।
हालाँकि पुराण (जो हमेशा बौद्धकाल के बाद के हैं) वाराणसी और काशी का विनिमयशील रूप से उपयोग करते हैं, वास्तव में, वाराणसी हमेशा से काशी जनपद की राजधानी रही है। जब गहड़वाल राजाओं ने वरुणा के पार एक किला बनाने, और पड़ोसी शक्तियों के लगातार हमलों से शहर की रक्षा करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने दो नदियों के संगम पर एक मजबूत किला बनाया, जो संयोगवश, शहर और उसके प्रमुख बाज़ार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी था। वरुणा नदी का उपयोग एक जलमार्ग के रूप में किया जाता था, जो आधुनिक विशेसरगंज बाज़ार की ओर जाता था, जो तब मच्छोदरी और मंदाकिनीतालाओ के किनारे स्थित था। पठार पर बना यह किला इतना मजबूत था कि बाद में इसे अंग्रेजी सेना ने भी उपयोग किया।
घनी आबादी वाला यह क्षेत्र कई महत्वपूर्ण मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से अधिकांश मंदिर नष्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ आज भी मौजूद हैं, जो हमें बेहतर समय की याद दिलाते हैं। इनमें शामिल हैं (1) नगर की रक्षक देवियाँ, वाराणस्या देवी और (2) काशी देवी, (3) खर्व विनायक, (4) राजराज विनायक, (5) महान लिंगम, आदि महादेव, और (6) आदि केशव। हालाँकि आसपास कोई भैरव रक्षक नहीं है, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि यहाँ आज भी एक श्मशान संचालित होता है, और सभी भैरव अनुयायियों के 'राजकुमार' दत्तात्रेय को यहाँ एक विशेष मंदिर में सम्मानित किया गया है।
'राजघाट' का नाम आज भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हालाँकि शहर खुद बहुत दूर दक्षिण की ओर खिसक चुका है। समय के साथ हुए तेज़ शहरी विस्तार के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि उत्तर का वन क्षेत्र, जो आध्यात्मिक साधकों द्वारा बसाया गया था, अब तक सौभाग्य से सुरक्षित रहा है। लेकिन अंततः, समय के जबड़े उसे भी निगल लेंगे।
VII
गहड़वालों ने इस स्थान को अपने किले के लिए चुनने का एक और महत्वपूर्ण कारण था। वरुणा नदी के एक मोड़ पर, मच्छोदरी के पास, प्राचीन काल में भरा-शिवाओं द्वारा निर्मित एक मिट्टी का किला मौजूद था। काशी के गण हमेशा अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति सजग रहते थे, जो नगरवासियों और मंदिर निर्माताओं द्वारा लगातार उल्लंघित किए जा रहे थे। भरा समुदाय ने हमेशा इस बात को महसूस किया कि उन्हें 'हीन' समझकर उपेक्षित किया जा रहा है। इस अपमान का उन्होंने हमेशा विरोध किया और अपने अधिकारों के लिए दृढ़ता से संघर्ष किया। भरा-स को अनदेखा करना कभी भी सुरक्षित नहीं साबित हुआ।
दूसरी ओर, मंदिर निर्माता 'असभ्य' लोगों को सभ्य बनाने के खेल में लगे हुए थे; और इस प्रक्रिया में, वे 'संस्कृति फैलाने' ("कुर्वन्तु विश्वम् आर्यम") के अपने पुराने उद्देश्य पर चल रहे थे। यह खेल वाराणसी के चारों ओर लगातार खेला जा रहा था। लेकिन वे अंततः भरा-शिवाओं को हटाने में असफल रहे और एक समझौते पर सहमत हो गए।
हम पहले ही देख चुके हैं कि वाराणसी की आम जनता, श्रमिक वर्ग, आज भी भरा-शिवाओं के प्राचीन गुणों को प्रदर्शित करती है। वे आज भी उन प्राचीन रुद्रियों की तत्परता और कठोर स्वभाव को धारण करते हैं, जिन्होंने कभी इस वन क्षेत्र के निवासियों के स्वभाव पर गहरा प्रभाव डाला था। प्राचीन 'रुद्र' आज भी वाराणसी के तथाकथित 'उग्र' लोगों की नसों में जीवित हैं, जैसा कि आज भी पांडवों, गंगापुत्रों, आभीरों के व्यवहार पैटर्न में देखा जा सकता है। यह स्वभाव अन्य स्थानीय समुदायों जैसे भंडा, मुरमी, केवट, कुम्हार, अहीर और डोम में भी देखा जाता है। इन समुदायों को आज भी वाराणसी में अनदेखा करना गंभीर नागरिक अशांति को जन्म दे सकता है।
नहीं, शिव-पशुपति-भैरव के अनुयायी आज भी वाराणसी के वातावरण पर उसी तरह हावी हैं जैसे प्राचीन काल में थे। वाराणसी में ब्राह्मणवाद ने वेदों की प्रतिष्ठा को एक अनूठी समन्वय प्रक्रिया के माध्यम से जीवित रखा है।
VIII
अब भी ऐसे कई प्रमाण हैं जो इस संघर्षपूर्ण स्थिति को उजागर करते हैं। ब्राह्मणवादी शक्तियों द्वारा स्थानीय लोगों और उनकी परंपराओं के दमन के प्रयासों ने वाराणसी के लोगों के चरित्र को गहराई से प्रभावित किया। आज, वही विशेषताएँ स्वयं ब्राह्मणवाद में भी समाहित हो गई हैं, जैसा कि वहाँ देखने को मिलता है।
स्थानीय राजकुमार धृतराष्ट्र और उनके वैदिक यज्ञ करने के प्रयास इस बात का उदाहरण हैं। वैदिक परंपरा द्वारा स्थानीय लोगों को समान रूप से स्वीकार न करने के कारण, स्थानीय लोग जिन्हें भैरव-शिव कहा जाता था, एक वैदिक विरोधी भावना विकसित करने लगे, चाहे ब्राह्मणों का प्रभाव कितना भी व्यापक क्यों न हो। यह तथ्य कि अधिकांश निवासी, यहाँ तक कि ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग भी, आसानी से शैव धर्म की ओर आकर्षित हो गए, इसका एक और संकेत है। कोई भी व्यक्ति नफरत और अपमान को अपनी विरासत के रूप में स्वीकार नहीं करता।
बाद में हम देखेंगे कि राजकुमार धृतराष्ट्र का यज्ञ बाधित कर दिया गया था। उन्हें सोमपान करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें बार-बार उनकी अनार्य जाति की याद दिलाई गई और उन्हें सीमित दायरे में रहने के लिए मजबूर किया गया।
जैसा कि हमने देखा, रुद्रवास अपनी भैरव-शिव परंपराओं के लिए जाना जाता था, जो हरिकेश और क्षेमक की वैदिक विरोधी परंपराओं के समान थीं। महामायूरी जर्नल में उल्लेख मिलता है कि दूसरी शताब्दी में रुद्रवास का अधिपति महाकाल (एक तांत्रिक देवता) था, जो एक यक्ष था (15.27.12)। हमने देखा कि हरिकेश, उद्भ्रम, विभ्रम, और स्वयं यक्षराज कुबेर ने भी गणों के प्रमुख पद को अपने लिए सुरक्षित रखा था। शिव भक्ति में परिवर्तित होने के बाद कुबेर गणेश पद तक पहुँचे और एक प्रकार से सीमाओं के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए।
ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब भैरव-शिवों ने केवल आर्यों के लिए आरक्षित अनुष्ठान किए। राजघाट की खुदाई से भैरव-शिवों के वैदिक परंपराओं पर प्रारंभिक नियंत्रण के प्रमाण मिलते हैं। वाकाटक अभिलेख के अनुसार, भैरव-शिवों ने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। (पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा ने इन्हें किया था। क्या ब्राह्मण लेखकों ने इस प्रकार अनार्य प्रयासों को मिटाने की कोशिश की थी?)
शिवलिंगोद्वहना राजवंशानाम... दशाश्वमेध-स्नानानाम भैरवशिवानाम...!
यह घटना प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट को एक महत्वपूर्ण अर्थ प्रदान करती है। यह लिंग पुराण और काशी खंड में ब्रह्मा द्वारा दस अश्वमेध किए जाने के संदर्भ को भी कुछ हद तक स्पष्ट करती है। वाराणसी के भारत कला भवन में एक खंडित प्रतिमा मौजूद है, जिसके सिर पर एक लिंग स्थापित है, जैसा कि भैरव-शिवों की परंपरा थी।
अभिलेख में वर्णित 'अवभ्रत' शब्द एक अनुष्ठानिक स्नान को दर्शाता है, जो किसी संकल्पित यज्ञ की पूर्णता के बाद किया जाता है।
हमें रुद्रसरोवर और ब्रह्मवास के बारे में भी जानकारी है। ब्रह्मवास वास्तव में एक छात्रावास था, जहाँ युवा ब्राह्मणों को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। बाद में, यह छात्रावास और सरोवर एक राम मंदिर और बाजार के निर्माण के कारण दब गए — और यह किसी इस्लामी आक्रमण का परिणाम नहीं था।
हमने मच्छोदरी चैनल-बेंड पर भैरव-शिवों द्वारा बनाए गए मिट्टी के किले का भी उल्लेख किया है। यह चैनल-बेंड हमारे शोध के लिए महत्वपूर्ण है, और हम बाद में इसके निहितार्थों पर चर्चा करेंगे।
स्थानीय निवासियों द्वारा वैदिक यज्ञों को अस्वीकार करने का विरोध भी दर्ज किया गया है, क्योंकि ब्राह्मण पुरोहितों ने उनके साथ सोमपान साझा करने से मना कर दिया था। यह आपसी भोजन, विवाह, और सामाजिक संबंधों पर लगी रोक आज भी ब्राह्मणों की पवित्रता की परंपरा को सुरक्षित रखती है।
भैरव-शिवों द्वारा ब्राह्मणवादी आडंबर और उच्चाधिकार के विरुद्ध प्रतिरोध कभी समाप्त नहीं हुआ। वाराणसी की संस्कृति निरंतर उथल-पुथल में रही, और अंततः शैव और गणेश उपासना को एक संतुलित सह-अस्तित्व का माध्यम बना लिया गया।
मूल निवासियों के लिए यह तनाव असहनीय हो गया था। उन्होंने हमेशा के लिए एक तीखा, विद्रोही दृष्टिकोण अपनाया, जो कथित 'उच्च संस्कृति' और विशिष्टता के समर्थकों के विरुद्ध बना रहा। शुद्ध आर्य परंपरा कभी भी उनकी प्रकृति से मेल नहीं खाई।
जैन-बौद्ध युग में जाति व्यवस्था की सीमाओं के विरुद्ध उठी आवाजों ने भी स्थिति में सुधार नहीं किया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध बहुत शोर मचा, और स्थानीय लोग अपनी युगों से चली आ रही रुद्र परंपरा के प्रति और भी रक्षात्मक हो गए। उनके लिए वर्णाश्रम की अवधारणा अस्वीकार्य थी। यह संभव है कि वाराणसी की बदनाम 'अराजकता', छल-कपट, दिखावे, डकैती, धमकी, और यहाँ तक कि हत्या की प्रवृत्ति — या परोपकारी बनने के दावेदारों के खिलाफ तत्काल आक्रामक रुख — वास्तव में इन्हीं ऐतिहासिक दमन की परछाइयाँ हों।
वन क्षेत्र के मूल निवासी धीरे-धीरे पहाड़ों से नीचे धकेले गए। वे दलदल, जंगल, और काशी के विस्तृत होते शहर की सीमाओं के उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी वीरानों में कठिन जीवन जीने को मजबूर हो गए।
IX
वाराणसी में गंगा के किनारे चलते हुए कभी-कभी कुछ अनपेक्षित, चट्टानी और कंकरीली पहाड़ियों के विस्तार मिलते हैं। ये पहाड़ियाँ विंध्य श्रेणी के अनियमित, उग्र विस्तार जैसी प्रतीत होती हैं।
हम जानते हैं कि पहाड़ियाँ और उनके शिलाखंडीय विस्तार हमेशा से जनजातीय समुदायों के प्रिय स्थल रहे हैं। वे अनदेखे देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ऊँची पहाड़ियों पर विशेष पूजा स्थलों की स्थापना करते हैं। इन विशिष्ट स्थानों में से अधिकांश एक देवी को समर्पित होते हैं, जहाँ विंध्यवासिनी उनकी प्रधान माता मानी जाती हैं। गया और हजारीबाग जिलों में भी इसी तरह की पहाड़ियों पर किसी न किसी धार्मिक स्मारक का मुकुट देखने को मिलता है। वाराणसी में शिव और माता सर्वोच्च देवता माने गए हैं, और तंत्र परंपरा यहाँ की वास्तविक मार्गदर्शक रही है।
गंगा की सतत पश्चिम-पूर्व धारा इन कंकरीली पहाड़ियों से बाधित होती है, जो मुख्यतः बलुआ पत्थर के ढेरों पर आधारित हैं। इस श्रेणी से बाधित होकर पूर्व की ओर बहती गंगा अचानक उत्तर की ओर मुड़ जाती है और फिर सोडेपुर में गोमती से मिलकर अपने पूर्व की ओर बहने के मार्ग को पुनः अपनाती है, जो मार्कंडेय और कैथी के आगे स्थित है।
हम इस पर्वत श्रृंखला पर वाराणसी के उन नामों के निहितार्थ खोज रहे हैं, जैसे — महास्मशान, गौरीपीठ, रुद्रवास, आनंदकानन, और अविमुक्त। क्या ये नाम आर्यों द्वारा धीरे-धीरे गैर-वैदिक, आदिम माता-पिता की संकल्पना को स्वीकारने, आत्मसात करने और सम्मानित करने की ओर संकेत नहीं करते? क्या इसे एक पुरुष-महिला के सह-अस्तित्व के रूप में नहीं देखा जा सकता, जिससे सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? यह अवधारणा इतनी सरल, वास्तविक और व्यावहारिक है कि यह वैदिक विचारधारा से मेल नहीं खाती।
चूँकि ये नाम संस्कृत में दर्ज हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये नाम उत्तर-आर्यकालीन होंगे। हम जानते हैं कि विजेता अक्सर अपने कब्जे वाली भूमि पर नए नाम थोपने के इच्छुक होते हैं। हालाँकि, वे मुण्डारी भाषा में 'गंग' शब्द को बदल नहीं सके, लेकिन उन्होंने उसे 'गंगा' नाम दिया और नदी के लिए कई वर्णनात्मक नाम जोड़ दिए। पुराने नाम जबरन कब्जे की कड़वी यादें संजोते हैं। आज भी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों के शहरों के नाम इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। सिकंदर ने भी कई शहरों के नाम बदलकर यूनानी नाम रखे ताकि उसके सैनिकों में अपने मूल देश की यादें बनी रहें। तुर्क, अफगान और मुग़ल आक्रमणकारियों ने भी भारत के कई शहरों के नाम बदले। महास्मशान और रुद्रवास के नाम भी शायद इसी प्रकार की ऐतिहासिक बाध्यताओं का परिणाम हैं।
समय के साथ नवागंतुकों ने रुद्र-जीवन शैली को आत्मसात कर लिया और धीरे-धीरे दोनों सांस्कृतिक धाराओं को एक प्रमुख प्रवाह में मिला दिया, जिसे 'सिन्धु धर्म' या 'हिन्दू धर्म' कहा गया — जो उन लोगों के जीवन दर्शन को परिभाषित करता था, जो सिंधु (इंडस) नदी के पार रहते थे।
वाराणसी के पशुपत, उमा-महेश्वर और कापालिक परंपराओं के प्रमाण के लिए अधिक खोज की आवश्यकता नहीं है। इन संप्रदायों से जुड़े जो मंदिर आज भी महास्मशान, आनंदकानन और समग्र वाराणसी में बिखरे हुए हैं, वे यह स्पष्ट करते हैं कि यह स्थान मूलतः ऐसे लोगों का था, जो वैदिक परंपराओं के विपरीत जीवन जीते थे।
निकुंभेश्वर और गोकर्णेश्वर जैसे गैर-वैदिक मंदिरों के अलावा, यहाँ क्षेमकेश्वर, दंत्तवक्त्र, और सोलह विविध गण-देव भी मिलते हैं, जिन्हें 'देव' कहा जाता था। बारा-देव आज भी गोधौलिया में एक पेड़ के नीचे स्थित है, जहाँ कभी गोदावरी नदी बहती थी, और जिसके आसपास अगस्त्य के पवित्र कुंड थे। शिव स्वयं को 'महादेव' यानी सभी देवों के देव के रूप में मान्य किया गया था।
वरुणा की सीमाओं के साथ स्थित विनायक मंदिरों के अलावा, यहाँ नंदिकेश्वर, कुटगण, पुष्पदंत जैसे महत्वपूर्ण गण-देव भी हैं। पुष्पदंत, गणेश मोहल्ला की ढलानों पर स्थित है, जिसे गणेश का निवास कहा जाता है।
हरिकेश और दिवोदास जैसी ऐतिहासिक-आधारित किंवदंतियों के माध्यम से, हमें उन समयों का पता चलता है, जब विष्णु (वैदिक धर्म) ने रुद्रों और यक्षों को खदेड़ा (जैसे मणिकर्णिका कथा में वर्णित है)। लेकिन ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी तक गण-शिव परंपरा पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी (हिरण्यकेशी गृहसूत्र और अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा)।
हमने पहले ही देखा है कि इस आपसी सह-अस्तित्व की प्रक्रिया ने वाराणसी के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। अनेक भैरव, गण, विनायक, और बीर से जुड़े मंदिर आज भी वाराणसी में मौजूद हैं। ये सभी मंदिर वाराणसी की रुद्र-शिव परंपरा की प्राचीनता के अमिट प्रमाण हैं।
अब इस चरण पर, हम वाराणसी की संस्कृति के तांत्रिक चरण की गहराई से पड़ताल करने का प्रस्ताव रखते हैं।
X
परंपरागत रूप से, वरुणा और असि इन दो धाराओं को कई रहस्यमय और काव्यात्मक व्याख्याओं के माध्यम से देखा गया है। ये व्याख्याएँ अक्सर चतुराईपूर्ण और कभी-कभी उत्तर-वैदिक भक्तों की भावनात्मक रचनाएँ प्रतीत होती हैं। पहाड़ियाँ, वनस्पति से आच्छादित भूमि और जलधाराएँ निश्चित रूप से आर्य आक्रमणों से भी पहले की हैं।
आज वाराणसी आने वाले पर्यटक और विद्वान, इन दो प्रसिद्ध धाराओं के अलावा, इस बात को भूल चुके हैं कि कई अन्य धाराएँ भी वाराणसी की पहाड़ियों को सिंचित करती थीं। इनमें से कुछ — जैसे मन्दाकिनी, गोदावरी, और धूतपापा — महत्वपूर्ण धाराएँ थीं, जिन पर कभी पुल बने होते थे। ये धाराएँ 1090 से लेकर 1290 तक सक्रिय थीं, और बाद में अकबर और औरंगज़ेब के समय तक इनका उल्लेख मिलता है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी इन धाराओं को देखा होगा।
ध्यान देने वाली बात है कि यह केवल ब्रिटिश कब्जे और उसके परिणामस्वरूप वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत पर हुए आघात के बाद ही हुआ, जब इन धाराओं को 'सौंदर्यीकरण' और 'स्वच्छता' के नाम पर बंद कर दिया गया! वे पुल, जो कभी इन धाराओं को जोड़ते थे, अब केवल नामों में ही जीवित हैं। अगस्ति पुल, देरसी (देवरी-शिव) का पुल, पुल-की-काली आदि नाम उन पुराने दिनों की मृदु याद दिलाते हैं।
पठान और मुग़ल, जो शुष्क और बंजर भूमि से आए थे, हमेशा से वृक्षों, धाराओं और झीलों के प्रति विशेष सम्मान रखते थे। उन्होंने प्रसिद्ध मंदिरों को लूटा और नष्ट किया, परंतु उनका उद्देश्य मुख्यतः सोने, चांदी और आभूषणों की संपत्ति हथियाना था। उन्होंने धार्मिक कट्टरता के चलते मूर्तियों को अपवित्र किया, लेकिन वे किसी सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य की स्थलाकृति को बिगाड़ना पसंद नहीं करते थे, जिसे वे सौंदर्य की दृष्टि से सराहते थे। वास्तव में, भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध बाग़-बगीचे इसी इस्लामी सौंदर्यबोध की देन हैं।
इसके विपरीत, इंग्लैंड से आई व्यापारी समुदाय ने कभी भी इस प्रकार की सौंदर्यपरक संवेदनाओं को महत्व नहीं दिया, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले से ही 'काले स्थानीय निवासियों' की भीड़ से भरे हुए थे।
5.एक नाव यात्रा
I
हमने वाराणसी को फिर से खोजने की यात्रा शुरू की। अब यह कार्य शुरू किया जा सकता था। इसके लिए, हमने वर्ष 1070 के आसपास एक काल्पनिक नाव यात्रा करने का विचार किया, जो वरुणा नदी के अधिकेशव बिंदु से लगभग दस मील आगे शैलेश्वर, आजमगढ़ रोड-जंक्शन, छावनी बस्ती और अर्दली बाजार के पीछे तक जाती है। इस यात्रा के दौरान, हम दोनों किनारों पर जीवन के धड़कते नाट्य को देखना चाहते हैं।
हम इस यात्रा का पूरी तरह से आनंद लेना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को वर्तमान शहर की मोहक सुंदरता से मुक्त करना होगा, जो आधे घेरे में पहाड़ियों पर बसा है। हमें उस आकर्षक अर्धचंद्राकार पर्वत-श्रेणी को भी भूलना होगा, जो नदी को उत्तर की ओर मोड़ने के लिए मजबूर करती है।
जब हम अपने मन को उस सम्मोहक आकर्षण से मुक्त कर लेंगे, तो हम अपनी आँखों को उस वास्तविक शहर की ओर मोड़ सकते हैं, जिसकी स्तुति युगों से भक्तों, तपस्वियों, संतों, विद्वानों और कवियों द्वारा की जाती रही है। इस प्रिय शहर की महिमा का गुणगान कभी थमा नहीं। जैन, बौद्ध और पुराण ग्रंथों में इसके लिए सुरंधना, सुदर्शन, पुष्पवती और रम्या (सुंदर) जैसे भावपूर्ण और काव्यात्मक नामों का वर्णन मिलता है।
इन मधुर नामों की तुलना में, वाराणसी के दक्षिणी क्षेत्र को एक अपेक्षाकृत शांत, अनार्य नाम से जाना जाता था — संकुर्ण, जो एक पिशाच या यक्ष का नाम है। (जो लोग भवभूति या भट्टनारायण के नाटकों से परिचित हैं, वे जानते हैं कि अनार्य पात्रों के लिए कैसे विचित्र नाम गढ़े जाते थे। स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने अनार्य वंश के पात्रों के लिए शूर्पणखा और कुम्भकर्ण जैसे नामों का प्रयोग किया।)
बुद्धघोष के अनुसार, कश्यप बुद्ध का जन्म वाराणसी में हुआ था, और उन्होंने मृगदाव में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वाराणसी और मृगदाव (सारनाथ) को अलग-अलग नगरों के रूप में देखा जाता था। बुद्धघोष के अनुसार, उस समय वाराणसी में मुख्य तीर्थस्थल गिने-चुने ही थे — मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, पंचगंगा, बरकारीकुंड, बिंदुमाधव और विश्वनाथ। केदारखंड का उस समय कोई उल्लेख नहीं मिलता।
यह दो महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर संकेत करता है:
1. मुख्य वाराणसी नगर मन्दाकिनी और मच्छोदरी के बीच की पट्टी में विकसित हुआ था, और जहाँ से गोदावरी बहती थी, वहाँ मुख्य चौक पहाड़ी थी।
2. इससे पता चलता है कि दशाश्वमेध और अगस्त्यकुंड के दक्षिण में स्थित नगर क्षेत्र अधिकतर अविकसित था, और इसे जानबूझकर एक वनाच्छादित पहाड़ी क्षेत्र के रूप में छोड़ दिया गया था।
इसका अर्थ है कि वास्तविक वाराणसी अत्यधिक जनसंख्या वाले ओंकारखंड में फली-फूली, जो वरुणा के तट पर फैला था, और आंशिक रूप से गंगा के किनारे त्रिलोचन-पंचगंगा तक फैला हुआ था।
आधुनिक वाराणसी के मनमोहक नदी किनारे की सुंदरता हमें प्राचीन काल के प्रसिद्ध शासकों — धन्वंतरि, हर्यश्व, वितहव्य, प्रतर्दन और दिवोदास के युग की सुंदरता से विचलित नहीं कर सकती। हमें याद रखना चाहिए कि आनंदकानन और रुद्रवास की ऐतिहासिक घटनाओं की तुलना में, राजघाट पर किले का निर्माण और उसका अधिग्रहण बहुत बाद की घटनाएँ हैं।
हम अपनी नाव यात्रा इस शहर के दोनों ओर फैले जीवन को देखने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुराना शहर वास्तव में गोमती के संगम से लेकर वरुणा के संगम तक और दक्षिण में मन्दाकिनी तालाब के किनारों तक फैला हुआ था। वास्तविक विश्वेश्वर पहाड़ी और भी ऊपर थी, जो नगर का शिखर बिंदु थी।
यह वही शहर था जिसे कोशल के राजा काश ने बसाया था। राजा काश के पोते धन्वंतरि थे, और उनके पोते दिवोदास ने 'रूखे' शिव (भारा) तत्वों को वाराणसी से बाहर करने की योजना बनाई थी, जिसके खिलाफ हैहय वंश के राजकुमार वितहव्य और हर्यश्व ने प्रतिरोध किया।
1027 ईस्वी के एक ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है कि कैसे हिंदू पुनर्जागरण ने लगभग बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंका था, लेकिन नबीपाल के शासन में इसे पुनः स्थापित किया गया। फिर 11वीं शताब्दी के अंत में कन्नौज के राजा चंद्रदेव (1072-96) ने शैव धर्म को फिर से स्थापित किया, और नव-बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरह मिटा दिया।
इस प्रकार, इस्लामी आक्रमणों से पहले वाराणसी में धार्मिक संघर्ष का नाटकीय इतिहास स्पष्ट रूप से सामने आता है। हम समझ नहीं पाते कि वह कौन-सी शक्तियाँ थीं जिन्होंने उस प्राचीन वाराणसी को नष्ट कर दिया, जिसका वर्णन बुद्ध ने किया था और जो सारनाथ के महान केंद्र के आसपास स्थित थी।
इस प्राचीन नगर का संहार इस्लामी हमलों से बहुत पहले हो चुका था। इसके प्रमाण आज भी बारकारीकुंड के आसपास के मंदिरों की वास्तुकला में देखे जा सकते हैं, जिन्हें बाद में इस्लामी सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। इन बचे-खुचे खंडहरों के भग्नावशेष आज भी बारकारीकुंड के पास की मस्जिदों में देखे जा सकते हैं।
इन सब साक्ष्यों से यह साबित होता है कि प्राचीन वाराणसी, विशेषकर ओंकारखंड, रुद्रवास और आनंदकानन, संतों के निवास स्थल थे, जिन्हें राजनीतिक परिवर्तनों से जानबूझकर अछूता रखा गया था।
आगे चलकर, जब गहड़वाल राजा चंद्रदेव (1080) ने अपनी किलेबंदी को दक्षिणी तट पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और एक मजबूत किला बनाया, तो व्यापारिक और संपन्न लोग भी दक्षिणी तट पर बसने लगे। इस प्रकार, वरुणा के उत्तरी तट का महत्व धीरे-धीरे कम होता गया।
हमें यह याद रखना चाहिए कि हालाँकि नए नगर में ज्यादातर 'शरणार्थी' बसे थे, लेकिन वे पवित्र पहाड़ियों की शांति और पवित्रता बनाए रखने के प्रति बेहद सतर्क थे। इसीलिए, ईसाई युग की दूसरी शताब्दी तक ये पहाड़ियाँ लगभग अछूती रहीं।
अंततः, शरणार्थियों की मुख्य बस्ती ओंकारखंड के उत्तरी भाग और विश्वेश्वरखंड के दक्षिणी छोर के बीच की भूमि पर बस गई। इसने वाराणसी की सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक धारा को सदियों तक बनाए रखा।
अब हमारी नाव यात्रा के दौरान, हम इस इतिहास की परतों को छूते हुए, उस शहर की झलक पाने की कोशिश करेंगे, जिसे युगों-युगों तक संतों, कवियों और भक्तों ने अपने शब्दों में अमर कर दिया।
II
जब हम वाराणसी के प्रमुख पवित्र मंदिरों, झीलों और नदियों पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये लगभग सभी त्रिलोचन पहाड़ी, ओंकारा पहाड़ी, बिंदुमाधव पहाड़ी और सबसे ऊँची, विश्वेश्वर पहाड़ी के आसपास स्थित थे।
यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। इस क्षेत्र को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा चिह्नित किया गया है:
1. पंचगंगा की पाँच नदियाँ
2. नगर की देवी काशी देवी
3. मंदाकिनी नदी और झील
4. मच्छोदरी जलग्रहण क्षेत्र
पूरे क्षेत्र को ओंकारखंड कहा जाता है। इस अत्यंत पवित्र भूमि, ओंकारखंड के भीतर, वाराणसी के लगभग सभी महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं: त्रिलोचन, कालभैरव, ओंकारेश्वर, कलेश्वर, त्रिपुर भैरवी, कालकूप, कृतिवासेश्वर, मध्येश्वर, अविमुक्तेश्वर, मंगलागौरी, दंत्तहस्त विघ्नेश्वर (बड़ा गणेश), विशालाक्षी, भवानी, संकट, वाराही, कपर्दीश्वर, बरकारीकुंड, बिंदुमाधव, अग्नेश्वर, वीरेश्वर, चंद्रेश्वर, ज्येष्ठेश्वर, भूतभैरव, मणिकर्णिका, चक्रतीर्थ, दंडपाणि, ललिता देवी, धुंडिराज, साक्षीविनायक, तारकेश्वर, धर्मेश्वर, मृत्युंजय।
यह सूची वाराणसी के तीर्थ यात्रा के दृष्टिकोण से हर महत्वपूर्ण स्थल को समेटे हुए है। इसकी तुलना में, केदारखंड में केदारनाथ के अलावा कोई बड़ा मंदिर नहीं है। दुर्गा या संकटमोचन जैसे मंदिर आधुनिक काल के हैं। केदारखंड में कुछ अपारंपरिक भैरव, बीर और तांत्रिक मंदिर हैं, जैसे बैजनाथ, बटुक भैरव, और कमच्छा। ये मंदिर उन स्थानों को दर्शाते हैं, जहाँ उमा-महेश्वर, वाममार्ग, पिशाच, और भूत संप्रदायों के साधक अपनी साधना किया करते थे। सौ साल पहले तक यह क्षेत्र घने जंगल से ढका हुआ था।
पश्चिम की ओर समतल भूमि पर पहुँचने पर, हम पिशाचमोचन झील और पितृकुंड पहुँचते हैं, जहाँ तीन वीर मंदिर हैं। कबीरचौरा से लेकर केदार पहाड़ियों तक, वर्तमान शहर की पश्चिमी सीमा के साथ चलते हुए, दशाश्वमेधेश्वर, भूतेश्वर, और गोदावरी के अलावा कोई प्रमुख मंदिर नहीं मिलता। इस नदी के पास अगस्त्येश्वर का उल्लेख काशी खंड में मिलता है।
केदार और हरिश्चंद्र घाटों के अलावा, इस क्षेत्र को काशी खंड में ज्यादा महत्व नहीं मिला है। कमच्छा से पश्चिम और गोधौलिया से पूर्व के बीच के क्षेत्र में विभिन्न आकार की झीलें और तालाब थे। वाराणसी का पूरा दक्षिण-पश्चिम भाग, जैसा कि हम आज जानते हैं, तब तक घने जंगलों से ढका हुआ था, जहाँ संत और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग एकांत साधनाओं के लिए अस्थायी आश्रम बनाते थे। इन जंगली आश्रमों के कुछ निशान छह-सात दशक पहले तक मौजूद थे।
वास्तव में, यह क्षेत्र बाद के मुगलों के समय तक काफी हद तक उपेक्षित था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। धार्मिक और व्यापारिक रुचि ने लोगों को वर्तमान शहर के उत्तरी किनारों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। घाटों और पहाड़ियों पर निर्माण कार्य 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ, ब्रिटिश शासन आने से कुछ समय पहले।
जब बाद के मुगल काल में दुर्रानी, अब्दाली और रोहिला आक्रमणों से परेशान सम्राटों को हिंदू सहयोग की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने कुछ रियायतें दीं। मराठा नेताओं को औरंगज़ेब और पठान शासकों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों के पुनर्निर्माण की अनुमति मिली। इससे वाराणसी की खोई हुई गरिमा वापस लाने का अवसर मिला। धार्मिक सिद्धांत तब पीछे छूट गए, जब एक साम्राज्य का भविष्य दांव पर था।
इस शाही अनुमति का लाभ उठाकर, वाराणसी के भव्य घाटों का निर्माण बड़ी तेजी से हुआ। भारत के हिंदू राजाओं ने एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए वाराणसी को फिर से सजाया, और नदी के किनारे उस युग की, या किसी भी युग की, सबसे शानदार और टिकाऊ संरचनाएँ खड़ी कीं। वाराणसी की नदी किनारे की वास्तुकला भारतीय निर्माण कौशल का जीवंत स्मारक है।
ये ऐतिहासिक घटनाएँ साबित करती हैं कि वाराणसी के प्रसिद्ध घाट अकबर के शासन से पहले अस्तित्व में नहीं थे। बौद्ध, मौर्य, थानेश्वर या शुंग अभिलेखों में वाराणसी के घाटों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। केवल कुछ नाम ही याद आते हैं — पंचगंगा, दशाश्वमेध (गहड़वालों के समय से प्रसिद्ध) और मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, जो आज एक श्मशान घाट है, पहले एक स्नान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध थी।
प्रश्न उठता है कि नए निर्माणों ने पारंपरिक वरुणा तट को क्यों छोड़ दिया? संभावनाएँ बताती हैं:
1. वरुणा नदी में सिल्ट जमा होने से मौसमी बाढ़ से तटों पर जलभराव होने लगा था।
2. पुराने मंदिर इतने नष्ट हो चुके थे, और इतनी मस्जिदें बन चुकी थीं कि पुनर्निर्माण अव्यावहारिक था।
3. कई हिंदू धर्मांतरित लोग अपने पैतृक घरों में रह रहे थे, और उन्हें हटाना सामाजिक और राजनीतिक रूप से असंभव था।
4. मच्छोदरी नाले के उपेक्षित होने से बिसेसरगंज बाजार तक की आसान नौका-यात्रा बंद हो गई। वर्तमान राजघाट (मालवीय ब्रिज के पास) अधिक व्यावहारिक लगा।
5. प्रह्लाद घाट, राम घाट और पंचगंगा घाट के बीच की ऊँचाई स्थापत्य दृष्टि से अधिक आकर्षक मानी गई।
वाराणसी के बिना घाटों वाला नदी किनारा कैसा दिखता होगा? कौन वहाँ रहता था? ऊँची पहाड़ियों का उपयोग कैसे होता था?
काशी खंड आनंदकानन श्रृंखला का वर्णन करते हुए कहता है कि ये पहाड़ियाँ आध्यात्मिक विद्यार्थियों के पसंदीदा स्थल थीं। यहाँ आश्रम फले-फूले। भूतेश्वर, ब्रह्मसरोवर, अगस्त्यकुंड और पातालेश्वर जैसे स्थान आज भी जीवंत लगते हैं।
इन पहाड़ियों पर किसी भी शहरी विस्तार ने अपनी अपवित्रता नहीं फैलाई थी। शांत गोदावरी नदी दशाश्वमेध घाट तक बहती थी और गंगा से मिलती थी। लगभग सभी घाटों के नाम हिंदू राजाओं के घरानों से जुड़े हैं, लेकिन दो अपवाद हैं — प्रसिद्ध चौसट्टी घाट, जिसे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के दुर्भाग्यशाली जमींदार प्रतापादित्य ने बनवाया था, और मनमंदिर घाट, जो राजा मानसिंह का स्मारक है।
यह घाट वास्तव में प्राचीन वाराही घाट था, जो आज के मीर घाट के करीब था, जो वास्तव में विश्वनाथ घाट है। इस क्षेत्र में वाराही, ललितासुंदरी, त्रिपुरेश्वरी, विशालाक्षी और कालिका की उपस्थिति इसकी तांत्रिक परंपरा की ओर इशारा करती है, विशेषकर वाममार्ग की।
इस प्रकार, वाराणसी के घाटों का वर्तमान वैभव सदियों की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उठा-पटक की विरासत है, जिसने इस महान नगरी को अनंत काल के लिए भारत की आध्यात्मिक राजधानी बना दिया।
III
जब हम वाराणसी के प्रमुख पवित्र मंदिरों, झीलों और नदियों पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये लगभग सभी त्रिलोचन पहाड़ी, ओंकारा पहाड़ी, बिंदुमाधव पहाड़ी और सबसे ऊँची, विश्वेश्वर पहाड़ी के आसपास स्थित थे।
यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। इस क्षेत्र को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा चिह्नित किया गया है:
1. पंचगंगा की पाँच नदियाँ
2. नगर की देवी काशी देवी
3. मंदाकिनी नदी और झील
4. मच्छोदरी जलग्रहण क्षेत्र
पूरे क्षेत्र को ओंकारखंड कहा जाता है। इस अत्यंत पवित्र भूमि, ओंकारखंड के भीतर, वाराणसी के लगभग सभी महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं: त्रिलोचन, कालभैरव, ओंकारेश्वर, कलेश्वर, त्रिपुर भैरवी, कालकूप, कृतिवासेश्वर, मध्येश्वर, अविमुक्तेश्वर, मंगलागौरी, दंत्तहस्त विघ्नेश्वर (बड़ा गणेश), विशालाक्षी, भवानी, संकट, वाराही, कपर्दीश्वर, बरकारीकुंड, बिंदुमाधव, अग्नेश्वर, वीरेश्वर, चंद्रेश्वर, ज्येष्ठेश्वर, भूतभैरव, मणिकर्णिका, चक्रतीर्थ, दंडपाणि, ललिता देवी, धुंडिराज, साक्षीविनायक, तारकेश्वर, धर्मेश्वर, मृत्युंजय।
यह सूची वाराणसी के तीर्थ यात्रा के दृष्टिकोण से हर महत्वपूर्ण स्थल को समेटे हुए है। इसकी तुलना में, केदारखंड में केदारनाथ के अलावा कोई बड़ा मंदिर नहीं है। दुर्गा या संकटमोचन जैसे मंदिर आधुनिक काल के हैं। केदारखंड में कुछ अपारंपरिक भैरव, बीर और तांत्रिक मंदिर हैं, जैसे बैजनाथ, बटुक भैरव, और कमच्छा। ये मंदिर उन स्थानों को दर्शाते हैं, जहाँ उमा-महेश्वर, वाममार्ग, पिशाच, और भूत संप्रदायों के साधक अपनी साधना किया करते थे। सौ साल पहले तक यह क्षेत्र घने जंगल से ढका हुआ था।
पश्चिम की ओर समतल भूमि पर पहुँचने पर, हम पिशाचमोचन झील और पितृकुंड पहुँचते हैं, जहाँ तीन वीर मंदिर हैं। कबीरचौरा से लेकर केदार पहाड़ियों तक, वर्तमान शहर की पश्चिमी सीमा के साथ चलते हुए, दशाश्वमेधेश्वर, भूतेश्वर, और गोदावरी के अलावा कोई प्रमुख मंदिर नहीं मिलता। इस नदी के पास अगस्त्येश्वर का उल्लेख काशी खंड में मिलता है।
केदार और हरिश्चंद्र घाटों के अलावा, इस क्षेत्र को काशी खंड में ज्यादा महत्व नहीं मिला है। कमच्छा से पश्चिम और गोधौलिया से पूर्व के बीच के क्षेत्र में विभिन्न आकार की झीलें और तालाब थे। वाराणसी का पूरा दक्षिण-पश्चिम भाग, जैसा कि हम आज जानते हैं, तब तक घने जंगलों से ढका हुआ था, जहाँ संत और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग एकांत साधनाओं के लिए अस्थायी आश्रम बनाते थे। इन जंगली आश्रमों के कुछ निशान छह-सात दशक पहले तक मौजूद थे।
वास्तव में, यह क्षेत्र बाद के मुगलों के समय तक काफी हद तक उपेक्षित था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। धार्मिक और व्यापारिक रुचि ने लोगों को वर्तमान शहर के उत्तरी किनारों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। घाटों और पहाड़ियों पर निर्माण कार्य 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ, ब्रिटिश शासन आने से कुछ समय पहले।
जब बाद के मुगल काल में दुर्रानी, अब्दाली और रोहिला आक्रमणों से परेशान सम्राटों को हिंदू सहयोग की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने कुछ रियायतें दीं। मराठा नेताओं को औरंगज़ेब और पठान शासकों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों के पुनर्निर्माण की अनुमति मिली। इससे वाराणसी की खोई हुई गरिमा वापस लाने का अवसर मिला। धार्मिक सिद्धांत तब पीछे छूट गए, जब एक साम्राज्य का भविष्य दांव पर था।
इस शाही अनुमति का लाभ उठाकर, वाराणसी के भव्य घाटों का निर्माण बड़ी तेजी से हुआ। भारत के हिंदू राजाओं ने एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए वाराणसी को फिर से सजाया, और नदी के किनारे उस युग की, या किसी भी युग की, सबसे शानदार और टिकाऊ संरचनाएँ खड़ी कीं। वाराणसी की नदी किनारे की वास्तुकला भारतीय निर्माण कौशल का जीवंत स्मारक है।
ये ऐतिहासिक घटनाएँ साबित करती हैं कि वाराणसी के प्रसिद्ध घाट अकबर के शासन से पहले अस्तित्व में नहीं थे। बौद्ध, मौर्य, थानेश्वर या शुंग अभिलेखों में वाराणसी के घाटों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। केवल कुछ नाम ही याद आते हैं — पंचगंगा, दशाश्वमेध (गहड़वालों के समय से प्रसिद्ध) और मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, जो आज एक श्मशान घाट है, पहले एक स्नान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध थी।
प्रश्न उठता है कि नए निर्माणों ने पारंपरिक वरुणा तट को क्यों छोड़ दिया? संभावनाएँ बताती हैं:
1. वरुणा नदी में सिल्ट जमा होने से मौसमी बाढ़ से तटों पर जलभराव होने लगा था।
2. पुराने मंदिर इतने नष्ट हो चुके थे, और इतनी मस्जिदें बन चुकी थीं कि पुनर्निर्माण अव्यावहारिक था।
3. कई हिंदू धर्मांतरित लोग अपने पैतृक घरों में रह रहे थे, और उन्हें हटाना सामाजिक और राजनीतिक रूप से असंभव था।
4. मच्छोदरी नाले के उपेक्षित होने से बिसेसरगंज बाजार तक की आसान नौका-यात्रा बंद हो गई। वर्तमान राजघाट (मालवीय ब्रिज के पास) अधिक व्यावहारिक लगा।
5. प्रह्लाद घाट, राम घाट और पंचगंगा घाट के बीच की ऊँचाई स्थापत्य दृष्टि से अधिक आकर्षक मानी गई।
वाराणसी के बिना घाटों वाला नदी किनारा कैसा दिखता होगा? कौन वहाँ रहता था? ऊँची पहाड़ियों का उपयोग कैसे होता था?
काशी खंड आनंदकानन श्रृंखला का वर्णन करते हुए कहता है कि ये पहाड़ियाँ आध्यात्मिक विद्यार्थियों के पसंदीदा स्थल थीं। यहाँ आश्रम फले-फूले। भूतेश्वर, ब्रह्मसरोवर, अगस्त्यकुंड और पातालेश्वर जैसे स्थान आज भी जीवंत लगते हैं।
इन पहाड़ियों पर किसी भी शहरी विस्तार ने अपनी अपवित्रता नहीं फैलाई थी। शांत गोदावरी नदी दशाश्वमेध घाट तक बहती थी और गंगा से मिलती थी। लगभग सभी घाटों के नाम हिंदू राजाओं के घरानों से जुड़े हैं, लेकिन दो अपवाद हैं — प्रसिद्ध चौसट्टी घाट, जिसे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के दुर्भाग्यशाली जमींदार प्रतापादित्य ने बनवाया था, और मनमंदिर घाट, जो राजा मानसिंह का स्मारक है।
यह घाट वास्तव में प्राचीन वाराही घाट था, जो आज के मीर घाट के करीब था, जो वास्तव में विश्वनाथ घाट है। इस क्षेत्र में वाराही, ललितासुंदरी, त्रिपुरेश्वरी, विशालाक्षी और कालिका की उपस्थिति इसकी तांत्रिक परंपरा की ओर इशारा करती है, विशेषकर वाममार्ग की।
इस प्रकार, वाराणसी के घाटों का वर्तमान वैभव सदियों की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उठा-पटक की विरासत है, जिसने इस महान नगरी को अनंत काल के लिए भारत की आध्यात्मिक राजधानी बना दिया।
IV
वर्तमान विश्वनाथ गली से शुरू होकर दशाश्वमेध रोड को पार करते हुए भूतेश्वर गली से केदार और हरिश्चंद्र घाटों तक जाने वाली भूमि की एक पट्टी है। हरिश्चंद्र रोड को पार करने के बाद, वही गली लंका और विश्वविद्यालय तक जाती है, प्राचीन काल के असी किले के पास असी पुल को पार करते हुए।
आज की वाराणसी की यह महत्वपूर्ण मुख्यधारा कभी पहाड़ियों के बीच एक पगडंडी भर थी, जो घने जंगलों से घिरी हुई थी। यह हमें अफगानों और मुगलों के युग की याद दिलाती है, जब यह एक पारंपरिक पगडंडी थी जो प्राकृतिक रूप से फैली पहाड़ियों के घने जंगलों को काटकर बनाई गई थी। आज भी ऐसे नाम — आइया-के-बरह, टेढ़ी नीम, बेलवरिया — उन दिनों की याद दिलाते हैं जब किसी स्थान को केवल वहाँ खड़े विशाल वृक्ष के आधार पर पहचाना जाता था। अब भी कई स्थानों के नाम वीर, गणेश, काली, या किसी प्राचीन बरगद के पेड़, या किसी पूजनीय कुएँ या तालाब के नाम पर रखे जाते हैं।
जब राजाओं ने वाराणसी को फिर से बसाना शुरू किया, तो उनका ध्यान इस हिस्से की ओर गया, जहाँ धार्मिक स्थलों के कारण कम से कम विरोध की आशंका थी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक ऐसा क्षेत्र चुना जहाँ विकास के खिलाफ धार्मिक आपत्तियाँ न उठें (अछूतों से दूर रहते हुए)। उन्होंने आनंदकानन पर्वत-श्रृंखला को चुना, जो दक्षिणी छोर पर हरिश्चंद्र के महास्मशान और उत्तरी छोर पर मणिकर्णिका से घिरी थी। वहाँ न तो मंदिरों की रक्षा करने वाले पुरोहित थे, न ही विस्थापित होने वाले लोग, और न ही व्यापारिक केंद्र चलाने वाले व्यापारी।
हो सकता है कि कुछ विनम्र धार्मिक भक्तों ने विरोध किया हो, जो प्राचीन काल से जंगल में बसे हुए थे। लेकिन भारा-शिव, हिंदू और बौद्धों के बीच लंबे संघर्षों के बाद, यह क्षेत्र काफी हद तक छोड़ दिया गया था। जो थोड़े-बहुत लोग वहाँ रह गए थे, वे पश्चिमी दलदलों की ओर चले गए — रेवतीकुंड (रेउरितालाब), बटुकनाथ, कमच्छा, खोजवाँ और गैवी की ओर।
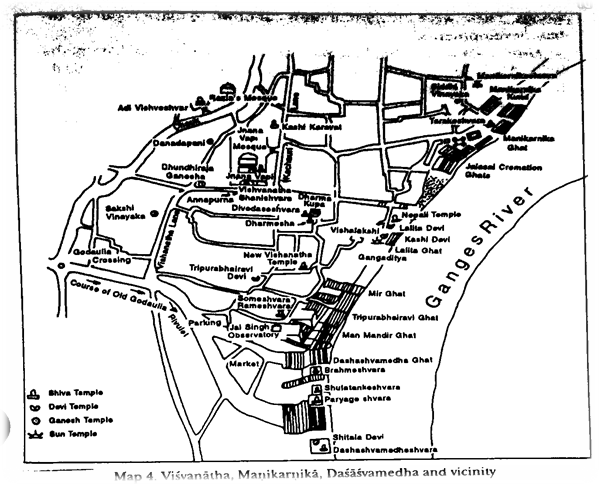
मानचित्र 4. विश्वनाथ, मणिकर्णिका, दशाश्वमेध और आसपास
राजसी आशीर्वाद और उनके कुशल इंजीनियरों और कारीगरों की मेहनत से, सत्रहवीं शताब्दी से ही नदी किनारे पर शानदार इमारतों की एक श्रृंखला खड़ी हो गई। राजनीतिक कारणों से निर्माण कार्य सौ साल के लिए रोक दिया गया, लेकिन सत्रहवीं शताब्दी के अंत में इसे फिर शुरू किया गया, और अठारहवीं शताब्दी के शुरू होने से पहले ही यह पूरा हो गया।
इस क्षेत्र के आसपास के लोग धीरे-धीरे पश्चिम की ओर उतरने लगे, जहाँ कई बड़े तालाब थे। इनमें सबसे बड़ा था रेउरितालाब, जो प्राचीन रेवती पुष्करिणी थी। इसी ढलान पर एक आधुनिक सड़क, विश्वविद्यालय रोड, बनी, जो चौक, गोधौलिया और विश्वविद्यालय को जोड़ती है। अंग्रेजों ने इस प्राचीन पगडंडी को चौड़ा और मजबूत किया। आज की मुख्य सड़क और प्राचीन गली लगभग समानांतर चलती हैं।
अगर हम एक पल के लिए आधुनिक इमारतों को हटा दें, तो हम शायद उन पहाड़ियों की कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें उस समय के चित्रकारों ने चित्रित किया था। इन चित्रों में सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी की वाराणसी की झलक मिलती है। लेखक ने स्वयं उन जंगलों के कुछ हिस्से देखे थे, जिन्हें अंधाधुंध काटकर शहरी विकास के लिए जगह बनाई गई।
संकटमोचन, बैजनाथ और शंकरमठ: मानसिक दृष्टि संकटमोचन, बैजनाथ, शंकरमठ, बेलवरिया, कोल्हुआ, गैवी, खोजवाँ और रेउरितालाब की ओर जाती है, जो हजारों ताड़ी के पेड़ों से घिरा हुआ था। यह क्षेत्र अक्सर अपराधियों का अड्डा बन जाता था, जहाँ लूट, हत्या, शराब और जुआ आम थे।
हालांकि, कुछ अपवाद भी थे। उदयपुर के राणा, इंदौर के होलकर और दरभंगा के महाराजा ने ठीक पहाड़ियों की चोटी पर निर्माण करवाया। उनके द्वारा बनाए गए लंबे सीढ़ीदार घाट आज भी उनकी वास्तु-कला और इंजीनियरिंग कौशल के साक्षी हैं। केदार घाट, राजा घाट, पर्रे घाट, चौसट्टी घाट, मुंशी घाट, अहिल्याबाई घाट, और उत्तर में मनमंदिर घाट की सीढ़ियों से आज भी पहाड़ियों की ऊँचाई का अंदाजा लगाया जा सकता है।
भैरव, नाग, और तांत्रिक परंपरा: उत्तर की ओर जाने वाले शरणार्थियों द्वारा इन पहाड़ियों से दूरी बनाए रखने का एक और कारण था — यह क्षेत्र भयावह भैरव, नाग, महेश्वर, कापालिक और कालमुख संप्रदायों के निवास के रूप में जाना जाता था। आनंदकानन के पतन के अंतिम दिनों में, ये पहाड़ियाँ अपराधी गिरोहों, ठगों और पेशेवर लुटेरों के लिए शरणस्थल बन गईं। महेश्वर और गणेश संप्रदाय के भक्त अपनी साधनाओं में किसी भी प्रकार की बाधा को सहन नहीं करते थे।
बटुक भैरव आश्रम और गणेश मोहल्ला जैसे स्थान इन संप्रदायों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। वाराणसी में आदि शंकराचार्य का एकमात्र तांत्रिक केंद्र भी इसी क्षेत्र में स्थित है। लेखक याद करते हैं कि 75 साल पहले तक वाराणसी के युवा अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रात के अंधेरे में अकेले इस जंगल को पार करने की चुनौती स्वीकार करते थे।
कहा जाता था कि यह क्षेत्र भूत-प्रेत, पिशाच, और विचित्र आत्माओं से भरा था, खासकर उन आत्माओं से, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। आज भी, इस क्षेत्र में एक तालाब है, जहाँ एक विचित्र परंपरा निभाई जाती है। हर साल एक विशेष दिन पर, सैकड़ों महिलाएँ निर्वस्त्र होकर इस पवित्र तालाब में स्नान करती हैं, संतान की प्राप्ति की कामना के लिए या संतान होने के लिए आभार प्रकट करने के लिए। यह तालाब सूर्यदेव लोलार्क को समर्पित है और इसे सार्वजनिक दृष्टि से छिपा कर रखा जाता है।
वाराणसी का आधुनिक विकास: अब यह क्षेत्र शहरीकरण से भर चुका है। कभी जो क्षेत्र जंगलों और दलदलों से भरा था, वहाँ आज अनगिनत कॉलोनियाँ, अस्पताल, कॉलेज, बिजलीघर, जल संयंत्र और पुलिस स्टेशन बन गए हैं। लेकिन घाट और तालाब, अपनी भव्यता के साथ, यह गवाही देते हैं कि मानव प्रयास ने प्राकृतिक वनों वाली पहाड़ियों की जगह शहरी विकास को थोप दिया।
फिर भी, पुराने दिनों की गूँज आज भी सुनाई देती है। गणेश मोहल्ला, अवधगर्भी, केनाराम-अस्थान, शंखोधरा, देवरिया-वीर, भोजू-वीर जैसे नाम उस रहस्यमय अतीत की याद दिलाते हैं। गणेश मंदिर, वीर मंदिर, सूर्य मंदिर और नरसिंह मंदिर, सब तंत्र और उमा-महेश्वर की वाममार्गी परंपराओं से जुड़े थे, जिन्हें कट्टर वैदिक परंपरा हमेशा शक की नजर से देखती थी।
इस प्रकार, वाराणसी के पहाड़, जंगल, और घाट एक ऐसी गाथा बुनते हैं, जहाँ धर्म, तंत्र, संघर्ष और पुनर्जागरण के असंख्य रंग आपस में घुल-मिल जाते हैं, और यह शहर अपनी अनूठी आध्यात्मिक पहचान को सदियों तक जीवित रखता है।
V
गंगा के किनारे फैली हुई यह पहाड़ी श्रृंखला, दक्षिण में चेतसिंह किले से लेकर उत्तर में मणिकर्णिका तक, मुख्य वन क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। आनंदकानन यहीं से शुरू होकर उन ढलानों तक फैला हुआ था, जिन्हें आज रेउरितालाब, लक्ष्मीकुंड, बेनिया और पिशाचमोचन के नाम से जाना जाता है।
यहीं पर भूतेश्वर मंदिर और भूतेश्वर तालाब स्थित था। अब ये स्थल अस्तित्व में नहीं हैं। फिर भी, तालाब की प्राचीन गहराई का कुछ अनुमान आज भी वहाँ की गोलाई में उतरने वाली सीढ़ियों से लगाया जा सकता है। पचास साल पहले तक, इस ढलान के किनारे तीन विशाल बरगद के पेड़ खड़े थे, जो एक गहरे तालाब के पास एक शांत उपवन बनाते थे।
आज वह स्थान एक सार्वजनिक सड़क और एक व्यस्त बाजार से ढक दिया गया है, और यह प्राकृतिक, शांतिपूर्ण परिदृश्य समय के साथ मिट गया है।
VI
गंगा के किनारे फैली हुई यह पहाड़ी श्रृंखला, दक्षिण में चेतसिंह किले से लेकर उत्तर में मणिकर्णिका तक, मुख्य वन क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। आनंदकानन यहीं से शुरू होकर उन ढलानों तक फैला हुआ था, जिन्हें आज रेउरितालाब, लक्ष्मीकुंड, बेनिया और पिशाचमोचन के नाम से जाना जाता है।
यहीं पर भूतेश्वर मंदिर और भूतेश्वर तालाब स्थित था। अब ये स्थल अस्तित्व में नहीं हैं। फिर भी, तालाब की प्राचीन गहराई का कुछ अनुमान आज भी वहाँ की गोलाई में उतरने वाली सीढ़ियों से लगाया जा सकता है। पचास साल पहले तक, इस ढलान के किनारे तीन विशाल बरगद के पेड़ खड़े थे, जो एक गहरे तालाब के पास एक शांत उपवन बनाते थे।
आज वह स्थान एक सार्वजनिक सड़क और एक व्यस्त बाजार से ढक दिया गया है, और यह प्राकृतिक, शांतिपूर्ण परिदृश्य समय के साथ मिट गया है।
घाटों के निर्माण के अलावा, पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानें भूतेश्वर बिंदु से केदार बिंदु तक लगभग अविकसित रहीं। इस क्षेत्र में पहला बड़ा परिवर्तन अठारहवीं शताब्दी के मध्य में आया। दशाश्वमेध से हरिश्चंद्र घाट तक की पहाड़ियों की संकरी पट्टी, बंगाल की एक ज़मींदार रानी भवानी के उपहारों के कारण बसने लगी, जिन्होंने 1753 में ब्राह्मणों को घर दान करने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण कराया।
आज यह स्थान बंगालीटोला के नाम से जाना जाता है, जहाँ आज भी रानी भवानी द्वारा बनवाए गए कई मंदिर खड़े हैं। जल्द ही, निचले बंगाल के कई अन्य ज़मींदारों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया और 'बंगालीटोला' क्षेत्र को और विस्तार दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि यह क्षेत्र तांत्रिक मंदिरों से भर गया — काली, तारा, भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी, जगद्धात्री, भद्रकाली, चतुष्षष्टि योगिनी के अलावा गोपाल, कृष्ण और भवानी के मंदिर भी स्थापित हुए।
दक्षिण भारत के धर्मनिष्ठ अमीरों के प्रयासों ने भी इस हिंदू पुनर्जागरण को मजबूत किया। महान जंगम स्वामी और आदि शंकर के अनुयायियों के संरक्षण में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और यहाँ तक कि मलयाली समुदायों ने तीर्थयात्रियों और गरीबों के लिए 'सत्र' (मुफ्त भोजनालय) खोले। अंततः यह क्षेत्र पहले से ही भीड़-भाड़ वाले वाराणसी का सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा बन गया।
हरिश्चंद्र घाट-शिवाला क्षेत्र के पूर्व और गैवी, कोल्हुआ, कमच्छा, शंकरमठ और सिगरा-रथतल्ला के पश्चिम के बीच के जंगलों में जो बदलाव आए, वे आज भी कई लोगों की जीवित स्मृतियों में बसे हुए हैं। वास्तव में, इस क्षेत्र में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि यह एक ओर विश्वविद्यालय तक फैल गई, और दूसरी ओर मारवाडीह रेलवे स्टेशन और उससे भी आगे बढ़ गई। यह वृद्धि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में तेजी से हुई।
VII
गंगा के किनारे फैली हुई यह पहाड़ी श्रृंखला, दक्षिण में चेतसिंह किले से लेकर उत्तर में मणिकर्णिका तक, मुख्य वन क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। आनंदकानन यहीं से शुरू होकर उन ढलानों तक फैला हुआ था, जिन्हें आज रेउरितालाब, लक्ष्मीकुंड, बेनिया और पिशाचमोचन के नाम से जाना जाता है।
यहीं पर भूतेश्वर मंदिर और भूतेश्वर तालाब स्थित था। अब ये स्थल अस्तित्व में नहीं हैं। फिर भी, तालाब की प्राचीन गहराई का कुछ अनुमान आज भी वहाँ की गोलाई में उतरने वाली सीढ़ियों से लगाया जा सकता है। पचास साल पहले तक, इस ढलान के किनारे तीन विशाल बरगद के पेड़ खड़े थे, जो एक गहरे तालाब के पास एक शांत उपवन बनाते थे।
आज वह स्थान एक सार्वजनिक सड़क और एक व्यस्त बाजार से ढक दिया गया है, और यह प्राकृतिक, शांतिपूर्ण परिदृश्य समय के साथ मिट गया है।
घाटों के निर्माण के अलावा, पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानें भूतेश्वर बिंदु से केदार बिंदु तक लगभग अविकसित रहीं। इस क्षेत्र में पहला बड़ा परिवर्तन अठारहवीं शताब्दी के मध्य में आया। दशाश्वमेध से हरिश्चंद्र घाट तक की पहाड़ियों की संकरी पट्टी, बंगाल की एक ज़मींदार रानी भवानी के उपहारों के कारण बसने लगी, जिन्होंने 1753 में ब्राह्मणों को घर दान करने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण कराया।
आज यह स्थान बंगालीटोला के नाम से जाना जाता है, जहाँ आज भी रानी भवानी द्वारा बनवाए गए कई मंदिर खड़े हैं। जल्द ही, निचले बंगाल के कई अन्य ज़मींदारों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया और 'बंगालीटोला' क्षेत्र को और विस्तार दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि यह क्षेत्र तांत्रिक मंदिरों से भर गया — काली, तारा, भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी, जगद्धात्री, भद्रकाली, चतुष्षष्टि योगिनी के अलावा गोपाल, कृष्ण और भवानी के मंदिर भी स्थापित हुए।
दक्षिण भारत के धर्मनिष्ठ अमीरों के प्रयासों ने भी इस हिंदू पुनर्जागरण को मजबूत किया। महान जंगम स्वामी और आदि शंकर के अनुयायियों के संरक्षण में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और यहाँ तक कि मलयाली समुदायों ने तीर्थयात्रियों और गरीबों के लिए 'सत्र' (मुफ्त भोजनालय) खोले। अंततः यह क्षेत्र पहले से ही भीड़-भाड़ वाले वाराणसी का सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा बन गया।
हरिश्चंद्र घाट-शिवाला क्षेत्र के पूर्व और गैवी, कोल्हुआ, कमच्छा, शंकरमठ और सिगरा-रथतल्ला के पश्चिम के बीच के जंगलों में जो बदलाव आए, वे आज भी कई लोगों की जीवित स्मृतियों में बसे हुए हैं। वास्तव में, इस क्षेत्र में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि यह एक ओर विश्वविद्यालय तक फैल गई, और दूसरी ओर मारवाडीह रेलवे स्टेशन और उससे भी आगे बढ़ गई। यह वृद्धि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में तेजी से हुई।
जब हम विदेशी आक्रमणों और धार्मिक स्थलों के विध्वंस की बात करते हैं, तो हमारा इशारा मुख्य रूप से नए नगर क्षेत्र की ओर होता है, जो 1080 में राजघाट किले की कथित सुरक्षा के तहत वरुणा के उत्तरी तट से दक्षिणी तट की ओर स्थानांतरित हुआ था।
इस्लामी आक्रमणों का प्रभाव दक्षिणी तट की बस्तियों पर कम ही पड़ा, क्योंकि लंबे समय तक चले ब्राह्मण-बौद्ध संघर्ष (विशेष रूप से शुंग और कण्व काल में) के कारण यह क्षेत्र पहले ही उजाड़ दिया गया था।
सबुक्तगिन, सिकंदर लोदी, महमूद शाह शर्की, या स्वयं औरंगजेब को भी सारनाथ के 'डोडो' के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब टोडरमल के पुत्र गोवर्धन ने चौखंडी के पास 'हुमायूँ के एक दिन के ठहराव' के स्मारक को खड़ा करने का निर्णय लिया, तब भी उन्हें मृगदाव या सारनाथ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
राजघाट पठार और उसका परिवेश, जो वरुणा पुल तक फैला हुआ है (नाते इमली, जगतगंज, क्वीन कॉलेज, लहुरा-वीर जैसी जगहों सहित), पुरातत्वविदों के लिए अत्यंत रुचिकर होना चाहिए। उन्हें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहाँ रेलवे पटरियाँ, स्टेशन, जेतपुरा और अलईपुरा जैसे मोहल्ले, और ग्रैंड ट्रंक रोड और बसंत कॉलेज परिसर का विस्तार हुआ है।

मानचित्र5: राजघाट पठार के साथ बनारस, जिसमें शुरुआती जल निकासी दिखाई गई है ।
यह क्षेत्र, ओंकारखंड के साथ मिलकर, बार-बार विदेशी आक्रमणों से तबाह हुआ। ये आक्रमण क्रमशः शैव और गणपति अनुयायियों, वैष्णवों और शैवों, हिंदू और बौद्धों, और अंततः मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा किए गए। अंततः, अंग्रेजों द्वारा सड़कों, रेलवे और पुलों के निर्माण के नाम पर यह क्षेत्र अपनी पहचान खो बैठा।
इसलिए, केवल मुसलमानों को विनाश का दोष देना एक सरलीकृत और पक्षपाती दृष्टिकोण होगा। मुस्लिम आक्रमण मुख्य रूप से ओंकारा और विश्वेश्वर खंडों तक सीमित थे। औरंगजेब ने विशेष रूप से धनवान मंदिरों जैसे विश्वेश्वर, ज्ञानवापी, बिंदुमाधव, ओंकारेश्वर, कृतिवास, मृत्युंजय, अविमुक्तेश्वर और बरकारीकुंड पर ध्यान केंद्रित किया — लूट के उद्देश्य से, धार्मिक उत्साह से नहीं।
इस अंध zeal ने अंततः मुगलों के पतन और यूरोपीय व्यापारियों द्वारा साम्राज्य के अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त किया। पवित्र स्थलों का अंधाधुंध विध्वंस आज भी हिंदू स्मृति में टीस की तरह चुभता है, विशेष रूप से उन स्थलों पर मस्जिदों के जानबूझकर निर्माण के कारण।
स्थानीय धर्मांतरित समुदाय, जिन्हें एक अभिमानी और असंवेदनशील सामाजिक व्यवस्था द्वारा लंबे समय तक घृणा की दृष्टि से देखा गया, इस दर्द को जीवित रखते हैं — जो एक जीवंत और विकसित समाज के लिए कोई भला नहीं करता।
VIII
गंगा के किनारे फैली हुई यह पहाड़ी श्रृंखला, दक्षिण में चेतसिंह किले से लेकर उत्तर में मणिकर्णिका तक, मुख्य वन क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। आनंदकानन यहीं से शुरू होकर उन ढलानों तक फैला हुआ था, जिन्हें आज रेउरितालाब, लक्ष्मीकुंड, बेनिया और पिशाचमोचन के नाम से जाना जाता है।
यहीं पर भूतेश्वर मंदिर और भूतेश्वर तालाब स्थित था। अब ये स्थल अस्तित्व में नहीं हैं। फिर भी, तालाब की प्राचीन गहराई का कुछ अनुमान आज भी वहाँ की गोलाई में उतरने वाली सीढ़ियों से लगाया जा सकता है। पचास साल पहले तक, इस ढलान के किनारे तीन विशाल बरगद के पेड़ खड़े थे, जो एक गहरे तालाब के पास एक शांत उपवन बनाते थे।
आज वह स्थान एक सार्वजनिक सड़क और एक व्यस्त बाजार से ढक दिया गया है, और यह प्राकृतिक, शांतिपूर्ण परिदृश्य समय के साथ मिट गया है।
घाटों के निर्माण के अलावा, पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानें भूतेश्वर बिंदु से केदार बिंदु तक लगभग अविकसित रहीं। इस क्षेत्र में पहला बड़ा परिवर्तन अठारहवीं शताब्दी के मध्य में आया। दशाश्वमेध से हरिश्चंद्र घाट तक की पहाड़ियों की संकरी पट्टी, बंगाल की एक ज़मींदार रानी भवानी के उपहारों के कारण बसने लगी, जिन्होंने 1753 में ब्राह्मणों को घर दान करने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण कराया।
आज यह स्थान बंगालीटोला के नाम से जाना जाता है, जहाँ आज भी रानी भवानी द्वारा बनवाए गए कई मंदिर खड़े हैं। जल्द ही, निचले बंगाल के कई अन्य ज़मींदारों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया और 'बंगालीटोला' क्षेत्र को और विस्तार दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि यह क्षेत्र तांत्रिक मंदिरों से भर गया — काली, तारा, भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी, जगद्धात्री, भद्रकाली, चतुष्षष्टि योगिनी के अलावा गोपाल, कृष्ण और भवानी के मंदिर भी स्थापित हुए।
ब्रिटिश शासन के दौरान वाराणसी के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया गया। उनकी उपेक्षा और अहंकार ने न केवल पवित्र स्थलों को नष्ट किया, बल्कि शहर की प्राचीन पहचान को भी मिटा दिया।
ब्रिटिश इंजीनियरों ने उन झीलों और नहरों को बंद कर दिया, जहाँ कभी धार्मिक गतिविधियाँ होती थीं — जैसे मच्छोदरी और मंदाकिनी। इन क्षेत्रों पर डाकघर, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, और सार्वजनिक भवन बनाए गए। रेलवे पटरियाँ बिछाई गईं, और गंगा पर स्टील का पुल बनाकर वाराणसी के पुराने भूगोल को पूरी तरह बदल दिया गया।
सबसे बड़ा नुकसान ऐतिहासिक प्रमाणों का हुआ। ओंकारखंड, विश्वनाथखंड, और मंदाकिनी नदी के अवशेष सड़कों, पुलों और रेलवे के नीचे दफन हो गए। लोगों की स्मृतियों से आनंदकानन और उसके प्राकृतिक आकर्षण धीरे-धीरे मिट गए।
फिर भी, वाराणसी कभी समाप्त नहीं हुई। इस शहर की आत्मा में फीनिक्स पक्षी की तरह पुनर्जन्म की शक्ति है। आज भी, वरुणा के तट पर भव्य मेले और उत्सव मनाए जाते हैं — रामलीला, नागपंचमी, गणेश चतुर्थी, मंगला गौरी, और पिशाचमोचन जैसे आयोजन लोगों की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाते हैं।
लोलार्क कुंड की विशेष परंपरा आज भी जीवित है, जहाँ महिलाएँ संतान प्राप्ति की कामना से स्नान करती हैं। यह अनूठा अनुष्ठान सूर्य पूजा की प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो शायद गंधार और कुषाण काल से वाराणसी में आई थी।
इतिहास की नजर से देखें, तो उत्सव और मेले ही उस संस्कृति की जीवंत निशानियाँ हैं, जिन्हें समय की धारा कभी मिटा नहीं सकती। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की प्रतिशोधी मानसिकता ने वाराणसी की धार्मिक आत्मा को कुचल दिया। उन्होंने न केवल पवित्र स्थलों को नष्ट किया, बल्कि स्थानीय लोगों की आस्था और सांस्कृतिक जड़ों को भी कमजोर करने का प्रयास किया।
वाराणसी की आत्मा तब टूटी, जब उसके जंगलों और नदियों को निर्ममतापूर्वक उजाड़ा गया। लेकिन यह शहर फिर भी जीवित रहा, और आज भी इसकी गलियों में इतिहास की गूँज सुनाई देती है — एक अजेय सांस्कृतिक विरासत की गाथा, जो बार-बार खंडहरों से उठकर नए सिरे से खिल उठती है।
6. वाराणसी का जन्म
I
गंगा के किनारे फैली हुई यह पहाड़ी श्रृंखला, दक्षिण में चेतसिंह किले से लेकर उत्तर में मणिकर्णिका तक, मुख्य वन क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। आनंदकानन यहीं से शुरू होकर उन ढलानों तक फैला हुआ था, जिन्हें आज रेउरितालाब, लक्ष्मीकुंड, बेनिया और पिशाचमोचन के नाम से जाना जाता है।
वाराणसी का जन्म
जो भी हिंदू संस्कृति के विकास को समझना चाहता है, उसके लिए वाराणसी का अध्ययन बेहद रोचक साबित होगा।
यह आवश्यक है कि हम प्राचीन समय की हवा को महसूस करें, और उस युग की धड़कनों को समझें। आत्मिक शांति और आध्यात्मिक लय को अपनी चेतना में उतारने के बाद ही हम पुनर्निर्मित वाराणसी की सही तस्वीर देख सकते हैं।
वाराणसी का विकास, वास्तव में, हिंदू संस्कृति के विकास का प्रतीक है।
हालाँकि, हमें वास्तविकता से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं।
बौद्ध, जैन, पुराण, महाकाव्य, तीर्थकल्प और गृहसूत्रों में, हमें वाराणसी की पहाड़ियों का काव्यात्मक वर्णन मिलता है, जहाँ गंगा नदी अपनी पूर्व दिशा से अचानक उत्तर की ओर मुड़ जाती है।
पश्चिमी तट धीरे-धीरे ऊँचा उठता है, जैसे आकाश को छूना चाहता हो। ये ऊँचे तट, जो चूनार और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार हैं, तीन प्रमुख शिखरों में विभाजित हैं। इन्हीं शिखरों को कवियों ने शिव के त्रिशूल के रूप में देखा, जिसके ऊपर पवित्र वाराणसी टिकी हुई है।
कहते हैं, शिव यहाँ अपनी शक्ति (सती) के साथ सृष्टि के आनंद में लीन रहते हैं। इस अनवरत एकता के कारण इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया — एक ऐसा स्थान, जहाँ कभी अलगाव नहीं होता।
प्राचीन काल में ये पहाड़ियाँ प्राकृतिक उपवनों और घने वनों से ढकी थीं। काशीखंड में पचास से अधिक श्लोकों में इन वनों के वृक्षों और उनकी पवित्रता का वर्णन है। यहाँ की शांति इतनी गहरी थी कि "चूहे बिल्लियों के कान कुतरते, और छोटे हिरण बाघिन से सुरक्षा की आशा करते।"
यह पूरा क्षेत्र देवी पार्वती का निजी निवास था। यहाँ केवल साधु, योगी और तपस्वी ही रह सकते थे। आम गृहस्थों के लिए यहाँ बसने की अनुमति नहीं थी। काशीखंड के अनुसार, यहाँ भूमि दान करना भी निषिद्ध था।
आनंदकानन में रहना, जैसे मंदिर के अंदर रहना। यहाँ शारीरिक, मानसिक, या वाचिक अशुद्धि की अनुमति नहीं थी। लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पहाड़ियों से नीचे, पश्चिमी दलदली क्षेत्रों में जाते थे।
स्थानीय भाषा में आज भी 'बाहर-जाना' या 'पर-जाना' का अर्थ नदी पार जाकर प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है — यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है।
गजनवी (1030 ईस्वी), गौरी (1144 ईस्वी) और शर्की (12वीं शताब्दी) के आक्रमणों ने वाराणसी की पवित्रता को भंग कर दिया। एक बार अपवित्रता फैलने के बाद, लोग शास्त्रों की मर्यादाओं को भूल गए। आक्रमणकारियों को हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुँचाकर विशेष आनंद मिलता था।
एक कथा के अनुसार, विवाह के बाद शिव और पार्वती अपने वैवाहिक आनंद में इतने लीन हो गए कि ब्रह्मांड की लय बिगड़ने लगी। देवताओं ने हिमालय की पत्नी मेनका से शिकायत की।
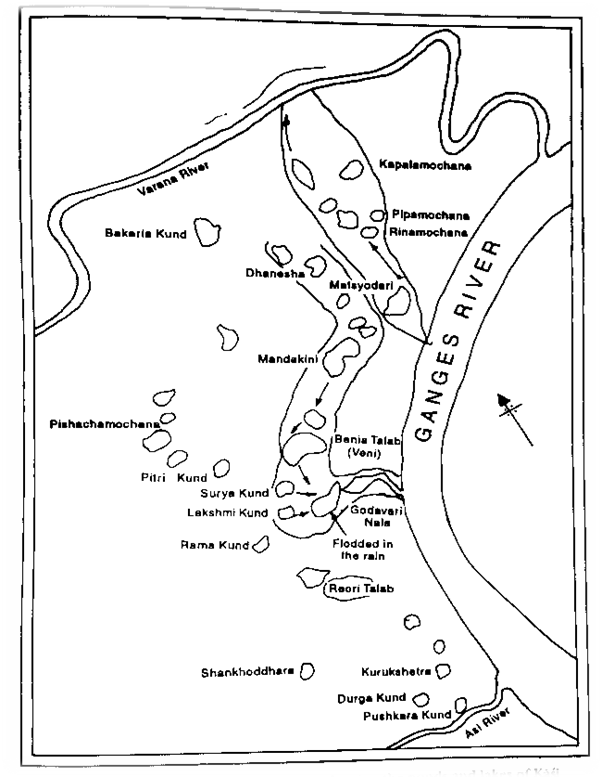
मानचित्र 6. जेम्स प्रिंसेप का बुनारस का मानचित्र, जिसमें काशी के तालाब और झीलें दिखाई गई हैं
मेनका ने पार्वती को समझाया कि उनके पति शिव एक नग्न योगी हैं, जो नागाओं, किरातों, गुप्त यक्षों, और सिद्धों के साथ रहते हैं — यह उनके कुल की मर्यादा के खिलाफ था।
पार्वती शर्मिंदा हुईं और शिव से एकांत की मांग की। तब शिव ने अपने गणों को एक ऐसा स्थान खोजने भेजा, जहाँ आर्य समाज के नियम न पहुँच सकें। इस तरह उन्होंने वाराणसी को अपने त्रिशूल पर स्थापित किया — एक ऐसा स्थान, जहाँ वे पार्वती के साथ सदा के लिए एक हो गए।
तांत्रिक भाषा में, आनंदकानन को सृष्टि की नाभि (Omphalos) कहा गया है — एक ऐसा रहस्यमयी केंद्र, जहाँ ऊर्जा (शक्ति) और पदार्थ (शिव) का अनवरत मिलन होता है, जिससे जीवन की निरंतर उत्पत्ति होती है।
काशीखंड में लिखा है:
"वह गहन अंधकार, जिसमें प्रकाश और उष्मा की संभावना छिपी थी, से सृजन की इच्छा उत्पन्न हुई। वही ऊर्जा, जिसे प्रकृति कहा गया, रूप धारण करने लगी। प्रकृति ने सृजन के लिए क्षेत्र (क्षेत्र) प्रदान किया — जिसे तांत्रिक परंपरा में योनि-मंडल कहा गया।"
इस प्रकार, वाराणसी केवल एक शहर नहीं है — यह सृजन और आनंद की सनातन ऊर्जा का केंद्र है।
इतिहास के उतार-चढ़ावों, आक्रमणों और विनाश के बावजूद, वाराणसी की आत्मा कभी नहीं मरी। यह शहर बार-बार राख से उठता है, एक नई ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण के साथ।
इसीलिए, वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है — एक ऐसा स्थान, जिसे कभी छोड़ा नहीं जाता।
II
और क्यों नहीं?
क्या यह आनंदकानन नहीं था? क्या यह अविमुक्त क्षेत्र नहीं था, जहाँ आर्य समाज की कठोर नैतिक पाबंदियाँ, सामाजिक प्रतिबंध, और अनुष्ठानिक बंधनों से परे एक स्वतंत्र जीवन की परंपरा थी? (पर्यङ्क-भूतं शिवयोः निरन्तर-सुखस-पदं)
आनंदकानन, इसके विपरीत, एक अत्यंत प्राचीन परंपरा का पालन करता था, जो ब्राह्मणवादी वैदिक बंधनों से कहीं अधिक पुराना और लोकप्रिय था। यह एक ऐसी समाज व्यवस्था को संजोए हुए था, जहाँ लोग मुक्त होकर जीते थे, और 'दो में एक और एक में दो' की आदिकालीन दिव्यता में पूर्णतः समर्पित थे। यह समाज प्रकृति के भयानक पक्षों को शांत करने के लिए किसी देवता की आराधना करने की बजाय, जीवन की मूलभूत आनंद-धारा में विश्वास रखता था।
यह जीवन शिव-गणों की भक्ति का मार्ग था — शिव का आनंदमय उद्देश्यपूर्ण जीवन। यहाँ मुक्ति का अर्थ था पूर्ण स्वतंत्रता, और इंद्रियों की रिहाई के माध्यम से आत्मा को ब्रह्मांडीय सृजन से जोड़ना। यह उनका मार्ग था — पूर्व-वैदिक, आदिकालीन मार्ग, जो जीवन की अनवरत धारा को ही परम सत्य मानता था।
नीनवे, बेबीलोन और खमेर से लेकर यूनान, मिस्र, साइप्रस, कन्नौज, मथुरा, उज्जयिनी, भृगुकच्छ, माहिष्मती, कालंजर, खजुराहो, कौशांबी और काशी तक, जीवन की ऊर्जा की आराधना एक सामूहिक श्रद्धा बन चुकी थी। यह वही भाव है, जो आज भी कालिदास, भास, अमरु, वत्स्यायन, अश्वघोष जैसे कवियों की कविताओं में गूंजता है।
आदिम युगल, शब्द और उनके अर्थ की तरह एकीकृत थे (वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे)। वे, भव और भवानी, शिव और शिवा, उमा और महेश्वर के रूप में आनंदकानन के नाम को एक दिव्य अर्थ प्रदान करते थे। यह वास्तव में उनका एकांत रमण-स्थल था — महेश्वर पंथ का रहस्यमयी कोना। यहाँ आदि तत्त्व जीवन-चक्र को घुमाने और उसे निरंतर विकसित करने के लिए ब्रह्मांडीय रमण में लीन थे।
यही आनंदकानन और रुद्रवास की उत्पत्ति थी — वह स्थान, जो यज्ञप्रिय वैदिक अनुयायियों के लिए भय और रहस्य का प्रतीक बन गया था। काशीखंड (26.4-6) इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। हम इसके कुछ श्लोक उद्धृत कर रहे हैं:
1. ततस्तदैकेलेनापि स्वैरं विहरत मया स्वविग्रहात् स्वयं सृष्टा स्वसरीरानुपायिनी। (XXVI.22-23)
2. युगपच्च त्वया शक्त्या सकं कालस्वरूपिणा मयाद्यपुरुषेणैतत् क्षेत्रं चापि विनिर्मितम्। (XXVI.24)
3. सा शक्ति: प्रकृतिः प्रोक्ता सः पुमान् ईश्वरः परः। ताभ्यां च रममाणाभ्यां तस्मिन् क्षेत्रे घटोत्भवः। (XXVI.24)
4. मुने प्रलयकालेऽपि न तत् क्षेत्रं कदाचन। विमुक्तं हि शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः। (XXVI.26)
5. आनंदकंद बीजानां अंकुराणि यथा ततः। श्रेयांसि सर्वलिङ्गानि तस्मिन् आनंदकानने। (XXVI.34-35)
6. आनंदकाननं शंभोः चक्रपुष्करिणीं हरेः। परब्रह्मैव सुक्शेत्रं लीलामोक्ष समर्पकम्।
इन श्लोकों का अर्थ यह है कि जब शिव अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने अपने ही स्वरूप से शक्ति को उत्पन्न किया, जिससे उन्हें आनंद की अनुभूति हो सके। दोनों ने मिलकर एक क्षेत्र (क्षेत्र) की रचना की — शक्ति के रूप में गतिशील काल और शिव के रूप में स्थिर ब्रह्म। इस क्षेत्र में, दोनों तत्त्व अनवरत ब्रह्मांडीय मिलन में लीन थे। भले ही ब्रह्मांड प्रलय में विलीन हो जाए, यह दिव्य मिलन कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए, इस क्षेत्र को 'अविमुक्त क्षेत्र' कहा गया — एक ऐसा स्थान, जहाँ शिव और शक्ति का मिलन कभी खंडित नहीं होता।
इस क्षेत्र को आनंदकानन कहा गया, जहाँ आनंद के बीज अंकुरित होते हैं, और कालांतर में नए जीवन के रूप में प्रकट होते हैं। यह शिव का 'आनंद उपवन' था, जहाँ जीवन का चक्र निरंतर घूमता रहता है। इस क्षेत्र का ध्यान करना, सृष्टि के रहस्यमय एकत्व का ध्यान करना है। यह क्षेत्र आत्मिक आनंद और सृजन के सौंदर्य के माध्यम से मोक्ष प्रदान करता है।
III
काशी की पवित्रता की प्राचीनता इसी गैर-वैदिक, पूर्व-आर्य तांत्रिक परंपरा में निहित है। वैदिक आर्यों के आगमन से पहले ही, वाराणसी में यह रहस्यमयी साधना व्याप्त थी। वैदिक लोग अपने यज्ञों और देवताओं के माध्यम से इस क्षेत्र को बदलने का प्रयास करते रहे, लेकिन शिव-भैरव परंपरा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि आर्यों को अंततः समर्पण करना पड़ा।
आज की वाराणसी उन्हीं संघर्षों और समझौतों का अंतिम परिणाम है। यहाँ गणों और भैरवों के मंदिर आज भी इस पवित्र संधि के स्मारक के रूप में खड़े हैं। पुराणों में वर्णित संघर्षों की कहानियाँ, हमेशा गण-भैरव मंदिरों की स्थापना के साथ समाप्त होती हैं। ये मंदिर आज भी वाराणसी की सुरक्षा के लिए प्रहरी के रूप में खड़े हैं।
इस सिद्धांत की साधना करने वाला साधक जीवन्मुक्त की अवस्था प्राप्त करता है — वह जो जीवन में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। 'आनंद' शब्द में वही रहस्य समाहित है, जो शिव-शक्ति के दिव्य मिलन में निहित है।
इसीलिए, वाराणसी को केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक चिरंतन सजीव प्रतीक मानना चाहिए — सृजन, आनंद, और आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक।
IV
मणि शब्द के तंत्र महत्व पर चुप रहना अनुचित होगा। मणि का बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील, यदि कोमल नहीं, तो गूढ़ अर्थ है। यह जैविक दृष्टि से भी अत्यंत अर्थपूर्ण है।
'ॐ मणि पद्मे हूं' वज्रयान में एक महत्वपूर्ण मंत्र रहा है। तंत्र योगियों के लिए कोई भी मंत्र अर्थहीन नहीं हो सकता। उसके अर्थ की व्याख्या पर जानबूझकर पर्दा डालना और भी बुरा होगा। शब्द विचारों को ढकते हैं। जब कोई विचार गूढ़ होता है, तो संबंधित अभिव्यक्तियाँ प्रतीकात्मक स्वरूप अपनाती हैं और चित्रलिपिक व्याख्याओं को प्रेरित करती हैं।
किसी भी स्थिति में, कोई विचार कितना भी अमूर्त क्यों न हो, उसे व्यक्त किया जाना चाहिए यदि मानवीय संचार को बनाए रखना है। आत्मनिष्ठ विचार स्पष्ट रूप से अव्यक्त होते हैं, लेकिन जब वे अभिव्यक्त होते हैं, तो उनकी संप्रेषणीयता में सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार की अभिव्यक्तियों से गूढ़ भाषा बनी होती है।
मणि एक ऐसा ही सूचक, चित्रात्मक और भावपूर्ण शब्द है, जो अपने छोटे से रूप में ज्ञान का एक विशाल संसार समेटे हुए है।
हम इस तथ्य से अवगत हैं कि तंत्र पुरुष और स्त्री साधकों के बीच घनिष्ठ संपर्क चाहता है, जो एक साथ साथी के रूप में कार्य करते हैं और एक विशेष योगासन में आलिंगन करते हैं। भास, कालिदास, भरतृहरी, भवभूति, बाणभट्ट, अश्वघोष, शूद्रक और कौटिल्य के अध्ययनकर्ता इस बात से परिचित हैं कि तंत्र, प्रेमासक्ति को सांसारिक मोह से मुक्त होने के लिए एक सहज साधन मानता है। यह परंपरागत मार्ग से हटकर चलने वाली विधि थी, जो केवल एक सिद्ध साधक के लिए थी। हाँ, केवल एक सिद्ध योगी के लिए ही अनुशंसित थी।
इस तरह की साधनाओं के साथ खिलवाड़ करना एक जिज्ञासु व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है! आदि काल से तंत्र प्रणाली शरीर की पूजा करता आया है, और शरीर से अधिक उस आंतरिक प्रेरणा की, जो एक से अनेक की सृष्टि के कार्य के लिए शरीर को प्रेरित करती है।
जीव-जगत को एक-दूसरे के शरीर की ओर आकर्षित करने और सृजन करने के लिए प्रेरित करने वाली यह शक्ति उसी स्रोत से आती है, जो पदार्थ को क्रियाशील बनाती है। यह मूल प्रेरणा ही वह रहस्यमय बिंदु है, जिसे तंत्र में परम श्रद्धा के साथ देखा जाता है, जो ह्लादिनी और चैतन्य (कामशक्ति और परम चेतना) के मिलन के रूप में पूजनीय है।
बहु-विस्तार के कार्य को संपन्न करने के लिए, शरीर—जो नश्वर है—एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है, जो इस नश्वर शरीर को अमरता प्रदान करता है। यह अपनी निरंतरता के माध्यम से 'अंत' को नकार देता है।
लेकिन, चूँकि यह एक शरीर है, यह आसानी से प्रलोभनों के जाल में फंस सकता है, जिससे विवेक और नियंत्रण की हानि हो सकती है। तंत्र शरीर को नियंत्रण की कठिन कला में प्रशिक्षित करता है।
इसी कारण तंत्र शरीर की पूजा करता है; और शरीर से अधिक उसकी प्राकृतिक इच्छाओं की, जिन्हें न तो कमजोरी माना जाता है और न ही दिव्य इच्छा से विचलन।
तंत्र नकारात्मक पथ को अस्वीकार करता है। तंत्र एक साथी की खोज करता है; और इस साथी का सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए: यह विपरीत लिंग का व्यक्ति हो सकता है, या ऐसा कोई जो पूरक आकर्षण रखता हो। इस आकर्षण को 'सेक्स-ड्राइव' या 'लिबिडो' कहा जाता है। इसे नियंत्रित करने वाला तत्व 'चैतन्य', 'प्रज्ञा' या 'एक उच्चतर चेतना की अवस्था' होता है। महायान तंत्र में प्रज्ञापारमिता को सर्वोच्च देवी माना जाता है, जिनकी कृपा के बिना 'सफलता' असंभव होती है।
इस संदर्भ में, स्त्री साथी एक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करती है और एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती है। पुरुष साथी का कार्य केवल क्षणिक होता है—उस क्षण को विद्युतित करने और बीज बोने का।
जीवन बीज की धारक होने के नाते, स्त्री शरीर और मन को गूढ़ परिवर्तनों के चक्र से गुजरना पड़ता है, जो अदृश्य से दृश्यमान रूप में विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया में अधिकांश शक्ति स्त्री शक्ति से प्राप्त होती है और वही इसे पोषित भी करती है।
स्त्री शरीर के इस विशेष भाग को, जिसे तंत्र में 'क्षेत्र', 'पट्टिका', 'तख्ती' या 'मंडप' कहा जाता है, एक उच्च सम्मान प्राप्त है। यह संकल्पना प्राचीन मिस्र, बाबेल, जापान, तिब्बत और चीन में भी प्रतिष्ठित थी। इस विषय पर सोचना, विश्लेषण करना और ध्यान करना ही इसे स्वीकार करना और सम्मान देना है।
स्त्री योनि, जिसे सामान्यतः वासना, अतिरेक और अश्लीलता के उपकरण के रूप में देखा जाता है, तंत्र और तंत्रियों के लिए 'माँ-मंडलम्', 'स्रोत', 'गर्भगृह' है। यही परम श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ से जीवन का उद्गम होता है। यह जीवन का स्रोत है, ज्ञान का द्वार है, उपलब्धियों का स्रोत है, और साधना एवं सिद्धि का आधार है।
जिस प्रकार एक किसान, माली, या वनस्पति-विज्ञानी, पुष्पों के परागण को महत्व देता है, ठीक उसी प्रकार तंत्र इस सृजन रहस्य को सम्मान देता है।
तंत्र का अध्ययन करते समय, हमें अपने मन को इस रहस्यमयी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः तैयार रखना चाहिए—केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए।
बिना 'बोधि' या 'अनुभूति' के, तंत्र उतना ही व्यर्थ है जितना कि एक भूखे बच्चे के लिए चित्रित स्तन। केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है; यह तो केवल प्रारंभिक चरण भी नहीं है; केवल अनुभव ही तंत्र साधना की परम परिणति है।
इस दृष्टिकोण से विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तांत्रिक सदैव एक स्त्री साथी पर जोर क्यों देता है और स्त्री को अपनी आत्मप्रतिबिंब, 'माँ', और 'सिद्धि' के रूप में क्यों सम्मानित करता है।
तंत्र कोई मनोरंजन नहीं है। तंत्र कोई व्यवस्थित पलायन नहीं है, जहाँ दुर्बल व्यक्ति रखैल या वेश्यावृत्ति के लिए विकल्प तलाश सके। कोई भी चालाकी तंत्र को दुरुपयोग का माध्यम नहीं बना सकती।
मादक पदार्थ तंत्र की अनुभूति उत्पन्न नहीं कर सकते; मदिरा इसके आनंद को ऊँचाई नहीं दे सकती; व्यभिचार इसकी दिव्य स्वतंत्रता और आत्म-संयम को सहायता नहीं कर सकता।
एक अपरिपक्व या असंयमित व्यक्ति के लिए यह ज्ञान हानिकारक हो सकता है। इसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और वह आत्म-विनाश की ओर बढ़ सकता है।
इसीलिए तंत्र के रहस्यों की रक्षा आवश्यक है। यही कारण है कि गुरु गोपनीयता पर जोर देते हैं। यह गोपनीयता रहस्यमयी नहीं, बल्कि एक सुरक्षात्मक प्रतिबंध है, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
इस प्रकार, 'मणि' शब्द तंत्र के गूढ़ भाषा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी व्याख्या करना स्वयं में एक साहसिक कार्य है। यह शब्द गूढ़ अर्थों से परिपूर्ण, संवेदनशील और कोमल है।
अतः, तंत्र में 'मणि' का महत्व केवल एक शब्द तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृजन प्रक्रिया की एक गहरी रहस्यमयी व्याख्या प्रस्तुत करता है।
V
मणिकर्णिका के बाद, हम महाश्मशान पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखते हैं, जो वाराणसी का एक और नाम है। इससे पहले हमने वाराणसी के नामों के संदर्भ में इस पर चर्चा की थी। यहाँ हम इस नाम पर ऐतिहासिक और गूढ़ दृष्टिकोण से विचार करेंगे।
श्मशान, जैसा कि हम जानते हैं, दाह-संस्कार स्थल होता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू समाज अपने दाह-संस्कार स्थलों को गाँवों और बस्तियों से बहुत दूर रखने का विशेष ध्यान रखता था। यह प्रदूषण से बचाव की एक सरल विधि थी।
यह एक और महत्वपूर्ण संकेत देता है कि हमारी वाराणसी, आनंद काननम, ऐतिहासिक काशी-वाराणसी शहर से काफी दूर स्थित रही होगी। काशी-वाराणसी का राजनीतिक महत्व विभिन्न राजवंशों के बीच विवाद का कारण रहा, जिनकी धार्मिक निष्ठाएँ भिन्न थीं। इसके अलावा, यह स्थान गौतम बुद्ध और जातक कथाओं में विशेष महत्व रखता था।
काशी में अब भी यह विश्वास बना हुआ है कि वरुणा और असी नदियों के बीच की संपूर्ण वाराणसी एक श्मशान स्थल है। इसकी सीमा के भीतर मृत्यु स्वयं ही मोक्ष की गारंटी मानी जाती है, चाहे अंतिम संस्कार किया जाए या नहीं, चाहे अंतिम विधियाँ संपन्न हों या नहीं। इस पवित्र भूमि की प्राकृतिक पवित्रता के कारण दाह-संस्कार को भी अनावश्यक माना जा सकता है।
महाश्मशान की इस महत्वपूर्ण अवधारणा को केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि यह समस्त जीव-जगत पर लागू होती है।
'स्म' का अर्थ होता है शव, और 'शान' का अर्थ है शयन, अर्थात् 'सदैव के लिए विश्राम'।
इस प्रकार, संपूर्ण वाराणसी एक विशाल 'शय्या' के रूप में कार्य करती है, जहाँ सभी मृत शरीर, चाहे उनका दाह-संस्कार हुआ हो या नहीं, अंतिम विश्राम पाते हैं।
और जब संपूर्ण सृष्टि का अंतिम विलय होगा, तब महाश्मशान में विश्राम प्राप्त कर चुके सभी शवों को अंतिम मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो यहूदी और ईसाई परंपराओं के 'पुनरुत्थान' के समान प्रतीत होता है।
वाराणसी के लोगों में दो लोकप्रिय मान्यताएँ हैं।
पहली मान्यता यह है कि यहाँ मृत्यु स्वयं मोक्ष की गारंटी है। जब अंतिम सांस समाप्त होती है और नश्वर शरीर वाराणसी की धूल में विलीन हो जाता है, तब प्राण अपनी मूल अवस्था को प्राप्त करता है।
दूसरी मान्यता स्थानीय लोगों के बीच गहरी आस्था रखती है। उनके अनुसार, वाराणसी की सड़कों पर पड़ा हुआ प्रत्येक पत्थर स्वयं भगवान विश्वेश्वर (महादेव) का लिंगस्वरूप है। इसी से कहावत प्रचलित है—'काशी के कंकर, सब ही शंकर'। इसलिए, जो कोई भी वाराणसी में रहने का चुनाव करता है, वह वास्तव में 'शिवता' अर्थात् शिव की स्थिति के सबसे निकट रहने का निर्णय करता है।
यद्यपि संपूर्ण क्षेत्र को नश्वर शरीरों के अंतिम विश्राम के लिए पर्याप्त माना जाता था, फिर भी वाराणसी का वास्तविक श्मशान घाट नदी के दक्षिणी छोर पर केदारखण्ड में स्थित था, अर्थात् वाराणसी की घनी आबादी से दूर। राजा चेत सिंह के किले और केदार घाट के बीच यह प्राचीन श्मशान स्थल स्थित था। इसे हरिश्चंद्र श्मशान के नाम से जाना जाता है, जहाँ कथाओं के अनुसार, अयोध्या के पौराणिक राजा हरिश्चंद्र ने वर्षों तक एक श्मशान रक्षक के रूप में सेवा की थी और इस स्थान को अपनी पहचान प्रदान की थी। (हालाँकि, यह लोकप्रिय मान्यता ऐतिहासिक प्रमाणों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।)
किन्तु आज के समय में, मणिकर्णिका श्मशान अधिक लोकप्रिय प्रतीत होता है।
VI
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मणिकर्णिका का श्मशान घाट के रूप में उपयोग अपेक्षाकृत हाल की बात है। पवित्र चक्रतीर्थ, ब्राह्मणाला और मणिकर्णिका तीर्थ के पड़ोस को अंतिम संस्कार के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। न तो काशी खंड और न ही काशी महात्म्य में इसका उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में मणिकर्णिका और चक्रतीर्थ दोनों को पवित्र 'स्नान' स्थल बताया गया है।
इसके अलावा, नदी तट का केंद्रीय स्थान स्वच्छता और सौंदर्यबोध की दृष्टि से इसे शवदाह स्थल बनाए जाने के विरुद्ध था। उपरोक्त तीन स्मारक सभी भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, और ऐतिहासिक विवशताओं के बिना इन्हें श्मशान भूमि के रूप में उपयोग नहीं किया जाता।
प्राचीन वाराणसी का परंपरागत श्मशान आदर्श रूप से आनंद काननम की तीन पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित था। यह हरिश्चंद्र घाट था, जो असी और केदार पहाड़ियों के बीच स्थित था।
वर्तमान मणिकर्णिका श्मशान घाट मूल रूप से राजवल्लभा घाट के नाम से जाना जाता था, और इसके निकटवर्ती स्नान घाट को जलेश्वर घाट कहा जाता था। इसके पास ही दत्तात्रेय घाट स्थित है, जिसके निकट ही दत्तात्रेय मंदिर है।
ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण जब अंतिम संस्कार के लिए किसी वैकल्पिक स्थान की खोज की गई, तो अपेक्षाकृत अलग-थलग पड़े 'रुद्र-खंड' को प्राथमिकता दी गई। उस समय यह क्षेत्र भीड़भाड़ से मुक्त था और इसे 'शहर का केंद्र' नहीं माना जाता था। ग्यारहवीं शताब्दी से पहले की वाराणसी, जैसा कि ज्ञात है, वरुणा नदी के किनारे फैली हुई थी और पंचगंगा पहाड़ियों तक विस्तृत थी।
तो फिर इस क्षेत्र को श्मशान भूमि के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? इसका उत्तर इतिहास में निहित है।
1824 में एक अंग्रेज़ (लेफ्टिनेंट कर्नल फॉरेस्ट) द्वारा बनाई गई मणिकर्णिका घाट की एक पेंटिंग में इस स्थान का सजीव चित्रण मिलता है। पृष्ठभूमि में तीन मंदिर, दो झुके हुए मंदिर (जलेश्वर मंदिर) जो आधे जल में समाए हुए थे, स्पष्ट रूप से अंकित हैं। इस चित्र में कहीं भी मानव बस्ती का कोई संकेत नहीं मिलता। इसके विपरीत, तट हरे-भरे वृक्षों से आच्छादित दिखाई देता है। वर्तमान में शवदाह के लिए प्रयुक्त चबूतरे और अधिरचनाएँ उस समय अनुपस्थित थीं।
इसका अर्थ है कि उस समय यह स्थान श्मशान के रूप में उपयोग नहीं किया जाता था। यहाँ शवदाह स्थल, उसके 'शांति स्तूप' और विश्राम मंडप का निर्माण हाल के समय की घटना है।
1760 में अवध के नवाब सफदरजंग के कोषाध्यक्ष लाला कश्मीरीलाल की माता का निधन हुआ। पार्थिव शरीर को हरिश्चंद्र घाट ले जाया गया, लेकिन वहाँ अंतिम संस्कार से जुड़े कर्मचारियों की मनमानी और अत्यधिक शुल्क वसूली के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से वह व्यथित हो गए। इसके विरोध में, उन्होंने इस स्थान का परित्याग कर दिया और एक नए स्थल की स्थापना का विचार किया, जहाँ आम जनता इस शोषण से मुक्त रह सके।
नया स्थल जलेश्वर घाट के निकट स्थित राजवल्लभा घाट को चुना गया, क्योंकि यह ब्राह्मणाला के पवित्र क्षेत्र के पास था। यह स्थान वाराणसी में नदी के किनारे सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता था। इसके अलावा, यह विश्वेश्वर पहाड़ी की तलहटी के निकट भी था।
1760 में कश्मीरीलाल की माता का अंतिम संस्कार वाराणसी के इस परम पवित्र स्थल पर किया गया। इस घटना के बाद से, चक्रतीर्थ और ब्राह्मणाला के निकट स्थित मणिकर्णिका को धीरे-धीरे अंतिम संस्कार के लिए अधिक पवित्र और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित स्थान के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
इसने अंततः हरिश्चंद्र घाट के कर्मचारियों की एकाधिकारवादी प्रथाओं को समाप्त कर दिया।
हमने पहले ही यह उल्लेख किया है कि परंपरागत रूप से संपूर्ण अविमुक्त क्षेत्र (विशेष रूप से विश्वेश्वरखंड) को महाश्मशान या अंतिम संस्कार स्थल के रूप में देखा जाता था।
इससे यह भी प्रमाणित होता है कि वाराणसी की पहाड़ियों, जहाँ केवल वन ही विद्यमान थे, विशेष रूप से नदी किनारे, गृहस्थों के निवास के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते थे।
यह इस प्रसिद्ध कहावत का समर्थन करता है कि "वाराणसी में कभी गृहस्थ निवास नहीं करते थे।" पहाड़ियाँ विशेष रूप से गणों, गैर-आर्य भूतनाथ, कालभैरव और गणपति के अनुयायियों द्वारा उपयोग में लाई जाती थीं।
यहाँ के भैरव संप्रदाय और वैदिक आर्यों के बीच तीव्र संघर्ष हुआ, जिसने काशी-कोसल और कन्नौज के गहड़वालों के बीच अनेक विवादों को जन्म दिया। जब अंततः शांति स्थापित हुई, तब ऋषि-मुनि, शिक्षक और उनके शिष्य इन पहाड़ियों पर आकर बसने लगे।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक श्मशान भूमि के स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान भी वाराणसी का वास्तविक नगर वरुणा नदी के दोनों किनारों और आस-पास के क्षेत्रों में विस्तृत था। कोसल के हमलों के कारण यह नगर दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता रहा, लेकिन इसका विस्तार विश्वनाथखंड के भीतर ही सीमित रहा।
इस नगर विस्तार के कारण दो अन्य श्मशान घाट समाप्त हो गए, जो नगर की परिधि में स्थित थे। इनमें से एक वरुणा-संगम के निकट और दूसरा दत्तात्रेय घाट के पास था।
नगर विस्तार के कारण ये श्मशान घाट समाप्त हो गए और मणिकर्णिका, भीड़भाड़ वाले नगर के मध्य स्थित एकमात्र प्रमुख अंतिम संस्कार स्थल बन गया, जो स्वास्थ्य संबंधी दावों को चुनौती देते हुए कर-शोषण को समाप्त करने का प्रतीक बन गया।
यह कहना गलत नहीं होगा कि वाराणसी की यह लड़ाई दो विरोधी विचारधाराओं के बीच थी—एक ओर गणों, भूतों, यक्षों और पिशाचों की सामाजिक रूप से स्वतंत्र और जातिविहीन शक्तियाँ थीं, तो दूसरी ओर वैदिक आर्य, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव और यज्ञीय परंपराओं को लागू करने का प्रयास किया।
यह रोचक है कि वाराणसी के दो प्रमुख देवता हैं—(1) शिव विश्वेश्वर, जो लिंग रूप में परम पुरुष का प्रतीक हैं, और (2) भवानी अन्नपूर्णा, जो सृजन की मूल ऊर्जा, ह्लादिनी, विशालाक्षी, विशाल या ललिता के रूप में स्त्री तत्व की उपस्थिति को दर्शाती हैं। कुछ लोग भवानी-अन्नपूर्णा को विश्वनाथ की अर्धांगिनी मानते हैं, लेकिन यह अधिकतर सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है।
वाराणसी के लिए यह संघर्ष वास्तव में प्राचीन परंपराओं और आधुनिक व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष था; यह स्वदेशी जीवनशैली और भक्ति परंपराओं की रक्षा के लिए वैदिक वर्ण व्यवस्था और यज्ञीय कर्मकांडों के विरुद्ध संघर्ष था। इसे मात्र एक ऐतिहासिक घटना या राजनीतिक-सामाजिक विस्तारवाद के संघर्ष के रूप में देखना भ्रामक होगा।
काशी के ययाति (प्रतर्दन, दिवोदास आदि) वैदिक वर्चस्व के समर्थक थे। महाकाव्यों और पुराणों में उनका उल्लेख विष्णु के अनुयायियों के रूप में किया गया है। उन्होंने वाराणसी की पहाड़ियों पर स्थित आनंद काननम में गणों के रुद्र संप्रदाय को समाप्त करने के लिए प्रयास किए, जिससे अन्य रुद्र-समर्थक शक्तियाँ उग्र हो गईं। इनमें 'कम-आर्य' हैहय, विदेशी क्षरता-पहलवाएँ, और प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शामिल थे, जिन्होंने वाराणसी की स्वतंत्र परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया।
इस प्रकार, वाराणसी की लड़ाई मूलतः विचारधाराओं की लड़ाई थी, जिसे इस पवित्र नगर के स्वाभाविक निवासियों ने लड़ा।
7. वाराणसी के खंडहर
I
हम जिन सामाजिक परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं, वे सामान्य सामाजिक परिवर्तनों की तरह क्रमिक नहीं थे। ये परिवर्तन दुर्भाग्यवश मानव लोभ, वासना और सत्ता प्राप्त करने की पशु प्रवृत्ति से उत्पन्न आघातों की प्रतिक्रिया के रूप में हुए।
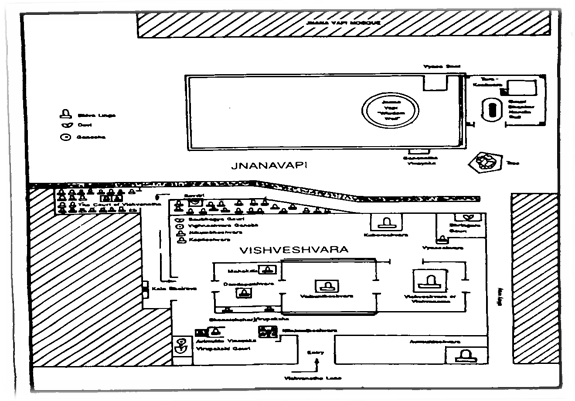
मानचित्र 7. ज्ञानवापी और मंदिर
यदि हम इस सामाजिक परिवर्तन के सूक्ष्म पहलुओं की जांच करें और वाराणसी के प्रमुख क्षेत्र, जिसे सामान्यतः 'चौक क्षेत्र' कहा जाता है, के नक्शे की सहायता लें, तो हमें इन तथ्यों से संबंधित और भी अधिक खुलासे मिल सकते हैं, जो उपर्युक्त टिप्पणियों का समर्थन करेंगे।
इस समय हमारी जांच को उस क्षेत्र तक सीमित किया जा सकता है, जो 'धुंडिराज-गणेश' से वर्तमान विश्वेश्वर मंदिर के उत्तर की ओर जाने वाली गली से घिरा हुआ है और त्रिपुरा भैरवी-कचौड़ी गली से मिलती है, जो नदी के समानांतर उत्तर-दक्षिण दिशा में जाती है। इस चौराहे से हम सीधे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जब तक कि हमें बाईं ओर एक द्वार नहीं मिलता, जिसे पार करके हम नगर कोतवाली (पुलिस मुख्यालय) पहुंचते हैं और फिर पश्चिम की ओर चौक चौराहे को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं।
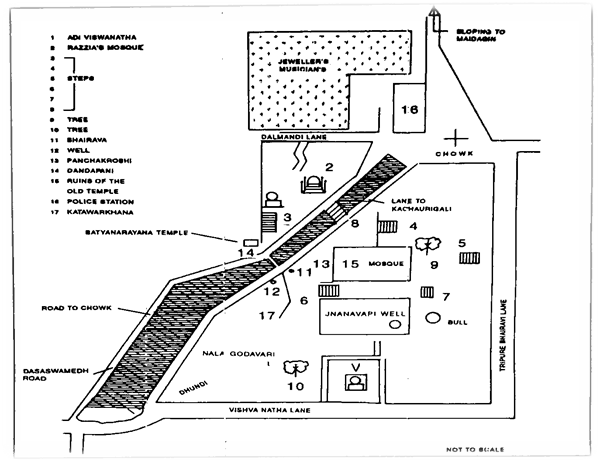
मानचित्र 8: चौक क्षेत्र-पुराने और नए मंदिर
हम पश्चिम दिशा में दलमंडी गली से होते हुए स्टेशन रोड तक पहुंचते हैं, जो बड़ियाबाग (जो पहले जेम्स प्रिंसेप के 1822 के नक्शे में 'बेनी' नाम से अंकित था) के पास एक विशाल झील थी। इस चौराहे से हम दक्षिण की ओर मुड़ते हैं और गोडौलिया क्रॉसिंग के पास एंग्लिकन चर्च तक पहुंचते हैं। वहाँ से हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं जब तक कि हम विश्वनाथ गली और दशाश्वमेध चौराहे (डेरसी का पुल) तक नहीं पहुंचते।
यह वर्गाकार क्षेत्र, जिसे हमने वर्णित किया, वाराणसी के हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है और इसे 'विश्वनाथखंड' या 'अंतरगृह' कहा जाता है।
वर्तमान मंदिर को केंद्र मानकर जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, तो हमें ज्ञानवापी का विस्तृत क्षेत्र मिलता है, जिसे 'ज्ञान का सरोवर' कहा जाता है।
काशीखंड के अध्याय 33 में ज्ञानवापी से संबंधित निम्नलिखित कथा दर्ज है: 'ईशान' (रुद्र) ने इस स्थान को उपयुक्त पाकर अपने प्रसिद्ध त्रिशूल से एक विशाल कुण्ड खोदा और इसके जल से संपूर्ण ब्रह्मांड को लिंग स्वरूप में स्नान कराया। हजारों कलश जल इस लिंग के अभिषेक के लिए प्रयुक्त हुए। रुद्र इससे प्रसन्न हुए और इस स्थान को आशीर्वाद देना चाहा। उन्होंने घोषणा की कि 'शिव' शब्द का अर्थ है 'परम ज्ञान की प्राप्ति', और इस प्राप्ति की अवस्था को जल रूप में मूर्त किया गया है, जिससे यह महान सरोवर भर गया। अतः यह जलाशय 'ज्ञानदा' या 'ज्ञानवापी' के नाम से जाना जाएगा।
काशीखंड के अध्याय 34 में 'रुद्र-शिव' के दो गणों, शुभ्रम (एक उलझा हुआ किंतु नेक आत्मा) और विभ्रम (एक भ्रमित और विपरीत आत्मा) का उल्लेख किया गया है। ये दोनों शिव के निवास पर प्रहरी थे। दंडनायक, या दंडपाणि, एक और विशिष्ट प्रहरी थे, जो इस जल की आध्यात्मिक शक्ति को दूषित करने वाली शक्तियों से रक्षा करने के लिए सदैव नियुक्त रहते थे।
शास्त्रों में, जब जल को शिव के आठ भौतिक रूपों में से एक कहा जाता है, तो विशेष रूप से इसी जलाशय का उल्लेख किया गया है। (जिसका अर्थ है कि इस कुण्ड का जल स्वयं शिव के स्वरूप के समान पवित्र था। इसमें स्नान करना पूर्णतः पापमुक्ति के समान था।)
हम यहाँ शास्त्रों के निर्देशों या उनके आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम इन कथाओं को अपने मार्गदर्शन के रूप में लेना चाहेंगे।
समकालीन लेखन हमें उस समय की सामाजिक मान्यताओं को समझने में सहायता करता है।
आज जैसा कि ज्ञानवापी का क्षेत्र अस्तित्व में है, यह हमारे लिए अत्यंत लाभकारी प्रमाण प्रस्तुत करता है। हमें इस स्थल को ध्यान में रखते हुए और पुराणों में वर्णित तथ्यों से इसकी पुष्टि करते हुए निष्कर्ष निकालने चाहिए।
वाराणसी की पुनः खोज के लिए मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं: (क) दक्षिण में वरुणा, (ख) मच्छोदरी चैनल और विशेष्वरगंज बाजार, (ग) मांडाकिनी तालाब, (घ) ज्ञानवापी और विश्वनाथ पहाड़ी।
विशेष रूप से ज्ञानवापी और विश्वनाथ पहाड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
प्राचीन नगर-रचना से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं की भी जाँच और व्याख्या की जानी चाहिए, जिससे तार्किक निष्कर्ष निकाले जा सकें।
समय के साथ कई विध्वंसकारी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध मंदिर का वास्तविक स्थान अनुमान का विषय बन सकता था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक विशाल सरोवर की उपस्थिति और उसका वास्तविक स्थान पूरी तरह से विवादास्पद नहीं हो सकता, विशेष रूप से जब अब भी एक स्थान को ज्ञानवापी के रूप में स्मरण किया जाता है, संरक्षित किया गया है और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है।
ज्ञानवापी अब भले ही जलाशय के रूप में अस्तित्व में न हो, लेकिन ज्ञानवापी अभी भी बनी हुई है। कुण्ड भर दिया गया है, लेकिन अब भी कुएँ से जल का छिड़काव किया जाता है।
इसलिए, हमें उपलब्ध ठोस प्रमाणों का लाभ उठाना चाहिए। पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में कई ऐसे प्रमाण हैं, जो महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकते हैं।
ज्ञानवापी के चारों ओर आज भी सीढ़ियों की एक श्रृंखला विद्यमान है। नक्शे में आठ सीढ़ी समूह दिखाए गए हैं, जिनमें से आठवें को छोड़कर सभी प्राचीन ज्ञानवापी, जो एक शास्त्रीय जलाशय था, के चारों ओर स्थित हैं। आज वहाँ केवल एक कुआँ बचा है, और श्रद्धालु इसे पवित्र मानते हुए इसके जल को सिर पर छिड़कते हैं या शुद्धिकरण के लिए ग्रहण करते हैं।
यही नहीं, पंडितों द्वारा सुनाई जाने वाली एक और कथा भी है। यह कथा कहती है कि जब महान मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, तो उसकी पवित्रता को 'यवनों' के स्पर्श से बचाने के लिए स्वयं 'महान लिंग' कुएँ में कूद गया।
लेकिन प्रश्न उठता है कि जो स्वयं अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए एक कुएँ में छिप जाए, वह आध्यात्मिक भ्रष्टता से कैसे बचा सकता है?
इस कथा की नैतिकता पर प्रश्न उठाया जा सकता है, लेकिन इसका ऐतिहासिक संदेश महत्वपूर्ण है।
इससे यह संकेत मिलता है कि मंदिर के वास्तविक लिंग को विध्वंस का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह पहले ही सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया गया था। यह कथा केवल वास्तविक लिंग को विध्वंसकों की पहुँच से दूर रखने के लिए बनाई गई थी।
इस प्रकार, वाराणसी में इतिहास, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन की गूढ़ परतों को समझने के लिए ज्ञानवापी क्षेत्र का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
II
वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर कुल कितनी बार नष्ट किया गया?
हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, पाँच बार।
1. पठान
ग़ोरी वंश (ग़ुलाम वंश): कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में
पहली बार इस मंदिर को
नष्ट किया।
2. खिलजी
वंश ने वाराणसी को विशेष रूप से
क्षति नहीं पहुँचाई। उत्तर भारत के अधिकांश
मंदिर पहले ही लूटे जा
चुके थे, इसलिए उन्होंने दक्षिण
के समृद्ध मंदिरों को निशाना बनाया। संभवतः
इसी दौरान लिंगम को परित्यक्त पहाड़ी पर
पुनर्स्थापित किया
गया। इल्तुतमिश (1210-36), जो एक समर्पित
सूफी था, ने मंदिर विध्वंस
की नीति को नहीं अपनाया।
लेकिन जौनपुर के शर्की सुल्तानों
(1390-1475) ने एक
बार फिर इस मंदिर को
नष्ट किया और वहाँ एक
मस्जिद का निर्माण किया। 1457 तक इस मंदिर
का कोई ऐतिहासिक उल्लेख उपलब्ध नहीं है।
ऐसा लगता है कि पूजा
किसी निकटवर्ती पहाड़ी पर जारी
रही।
3. तुगलक
वंश के शासनकाल में फिर से वाराणसी
को आघात सहना पड़ा। फिरोज
शाह तुगलक (1351) ने निकटवर्ती पहाड़ी
पर बने नए मंदिर को
ध्वस्त कर दिया।
4. लोधी
वंश (1451-1526): सिकंदर
लोधी ने उसी स्थान पर
पुनर्निर्मित मंदिर
को पुनः नष्ट कर दिया
और आगे वहाँ मंदिर निर्माण
की अनुमति नहीं दी।
5.
मुगल वंश: अंततः जब अकबर
ने मंदिर के पुनर्निर्माण की
अनुमति दी, तो ज्ञानवापी स्थल
पर एक नया मंदिर बनाया
गया। इसे 1679 में औरंगज़ेब ने
नष्ट कर दिया।
[संभवतः यही वह लिंगम था, जिससे 'कुएँ में कूदने' की कथा शुरू हुई, जब इसे वास्तव में गुप्त रूप से कहीं और ले जाया गया था।]
दिल्ली पर शासन करने वाले लगभग सभी इस्लामी वंशों ने मंदिरों को लूटने का प्रयास किया।
खिलजी वंश, जिसने वाराणसी को सीधे क्षति नहीं पहुँचाई, वैसे भी मंदिर विध्वंस के लिए कुख्यात था। हिन्दू मंदिरों पर उनके आक्रमणों का मुख्य कारण आर्थिक था। मंदिरों को लूटने का अर्थ था धन प्राप्त करना। विशाल खज़ाने उन शासकों के लिए अत्यधिक आकर्षक थे, जिन्हें अपनी विशाल सेनाओं को संतुष्ट रखना पड़ता था, जबकि वे अनियमित वेतन प्रणाली से ग्रस्त थे। उस समय एक संगठित वेतनभोगी स्थायी सेना का अस्तित्व नहीं था।
यहाँ तक कि उच्च पदस्थ जनरलों को भी नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। अधिकारियों को केवल उपाधियाँ और 'जागीरें' दी जाती थीं, जो न तो बेची जा सकती थीं, न स्थानांतरित की जा सकती थीं, न ही वंशानुगत रूप से हस्तांतरित की जा सकती थीं। जागीरें पूरी तरह से शासक के आनंद पर निर्भर थीं।
इस स्थिति में, सैनिकों को लूट से प्राप्त हिस्से से संतुष्ट रखना आवश्यक था। हिन्दू मंदिरों में सदियों से संचित धन इन शासकों के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन था। धर्म केवल एक बहाना था, जिससे जनता को 'काफ़िरों' के विरुद्ध भड़काकर इस लूट को वैध ठहराया जा सके।
यही कारण है कि ऐतिहासिक शोधकर्ता लूटपाट करने वालों के धार्मिक उद्देश्यों पर संदेह करते हैं। प्रत्येक मंदिर लुटेरों के लिए एक आसान लक्ष्य था। जब भी वेतन न मिलने से सेना में असंतोष बढ़ता, तो धार्मिक उन्माद भड़का दिया जाता और किसी न किसी मंदिर को निशाना बनाया जाता। यह उन भयानक समयों की क्रूर सच्चाई थी।
[अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली की लूट और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के बीच सक्रिय कुख्यात ठगों का उदय भी इसी 'लूट और भुगतान' या 'लूट और बंटवारा' प्रणाली से जुड़ा था।]
खिलजी वंश ने उत्तर भारत में अधिक मंदिर नष्ट नहीं किए, क्योंकि पहले ही लगभग सभी प्रमुख मंदिर ध्वस्त किए जा चुके थे।
पेशावर (पुरुषपुर) के महान बौद्ध केंद्र, बारामूला (वराहमूला) और मुल्तान के विशाल मंदिर, कश्मीर, राजस्थान और सौराष्ट्र के समृद्ध मंदिर, सोमनाथ का भव्य मंदिर, इंद्रप्रस्थ (दिल्ली) के राजा अनंगपाल का सूर्य मंदिर, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, गया, खजुराहो, पुरी और भुवनेश्वर के प्रमुख मंदिर सभी पहले ही नष्ट कर दिए गए थे।
उत्तर भारत में अब लूट के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए दक्षिण को निशाना बनाया गया। दक्षिण में महान हिंदू सम्राटों द्वारा संरक्षित भव्य मंदिर थे। चालुक्य, चोल, पांड्य, होयसाल, राष्ट्रकूट, सातवाहन, काकतीय, पहलव और कलचुरी सभी मंदिर निर्माण में अग्रणी थे। इन मंदिरों के माध्यम से न केवल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता था, बल्कि कला, कलाकारों, विद्या और शिक्षा की रक्षा भी की जाती थी।
इन मंदिरों में संचित विशाल संपत्ति उन शासकों की लालसा को बढ़ाती थी, जो किसी भी तरह अपनी सेनाओं को संतुष्ट रखना चाहते थे। इसलिए धर्म के नाम पर इन मंदिरों की लूट को एक अनुष्ठान की तरह अपनाया गया।
किसी भी धर्म ने लूट, हिंसा, बलात्कार और अत्याचार की अनुमति नहीं दी, विशेष रूप से इस्लाम ने तो बिल्कुल नहीं।
मंदिर विध्वंस का इतिहास निनेवेह, उर, पर्सेपोलिस, बेबीलोन, मदीना, मक्का, काहिरा, डार्डानेल्स से लेकर पुरुषपुरा, मूलस्थान, वराहमूला, मार्तंड, चिन्णकेशव, परिहासकेशव (कश्मीर) और वाराणसी तक, सदा एक जैसी कहानी कहता आया है। मंदिरों के विध्वंस ने धार्मिक उन्माद को हवा दी और लुटेरों की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा।
इसीलिए जब उत्तर भारत में मंदिरों की लूट संभव नहीं रही, तब खिलजियों की निगाहें दक्षिण भारत की ओर मुड़ गईं।
एक तबाह वाराणसी 150 वर्षों तक अपने हाल पर छोड़ दी गई। 150 वर्षों तक शहर पर एक महाश्मशान जैसी शांति छाई रही, जबकि नया नगर पुनरुद्धार की प्रतीक्षा करता रहा।
यह मंदिरों की लूट और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कुचलने की प्रक्रिया केवल तीन कालखंडों में रुकी। ये काल थे: (1) इल्तुतमिश-बलबन (1266-87) (2) महान सम्राट अकबर (1556-1605) (3) सम्राट शाह आलम (1772)
रेखांकन
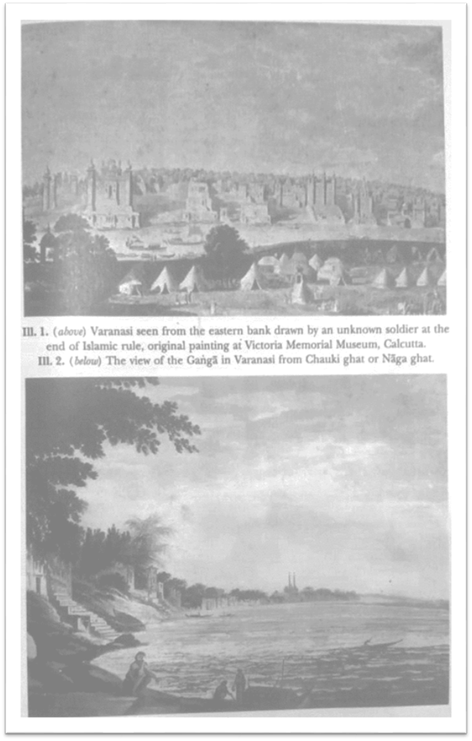
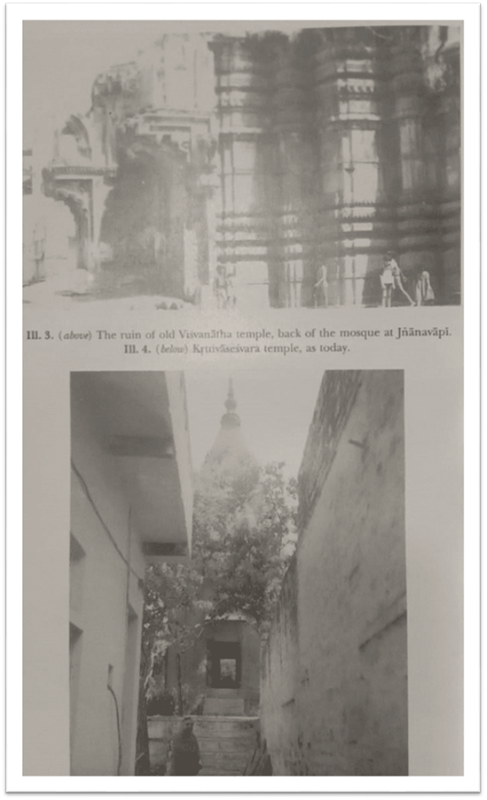
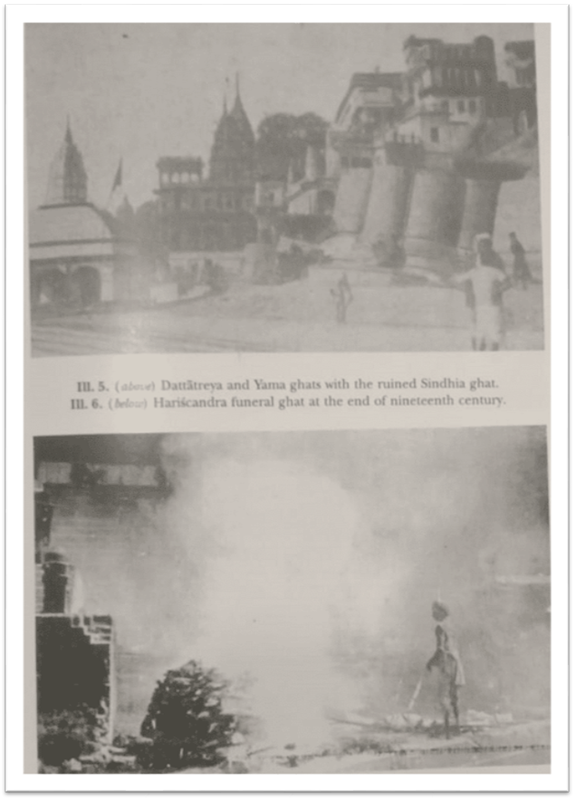
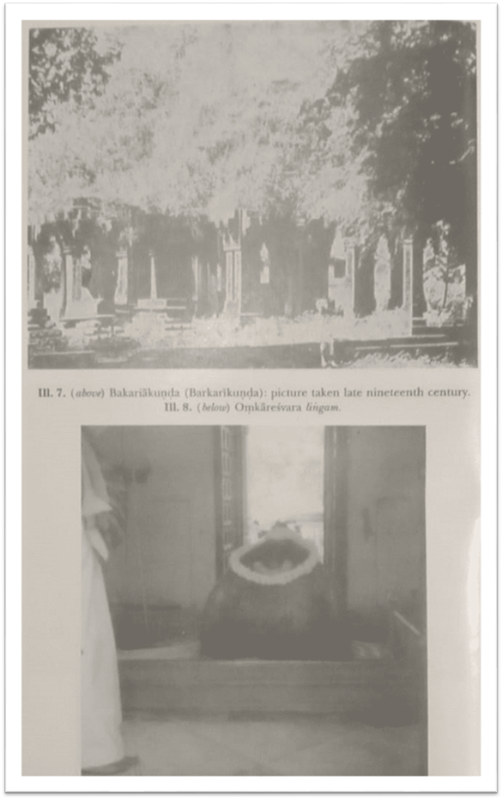
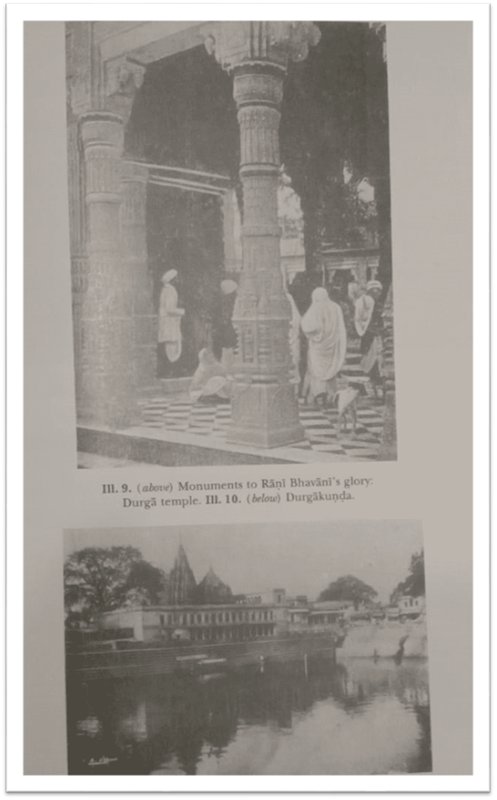
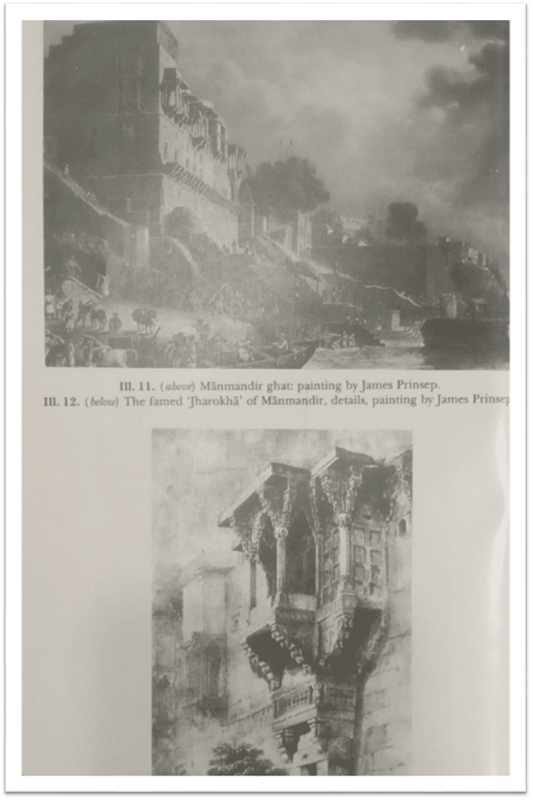
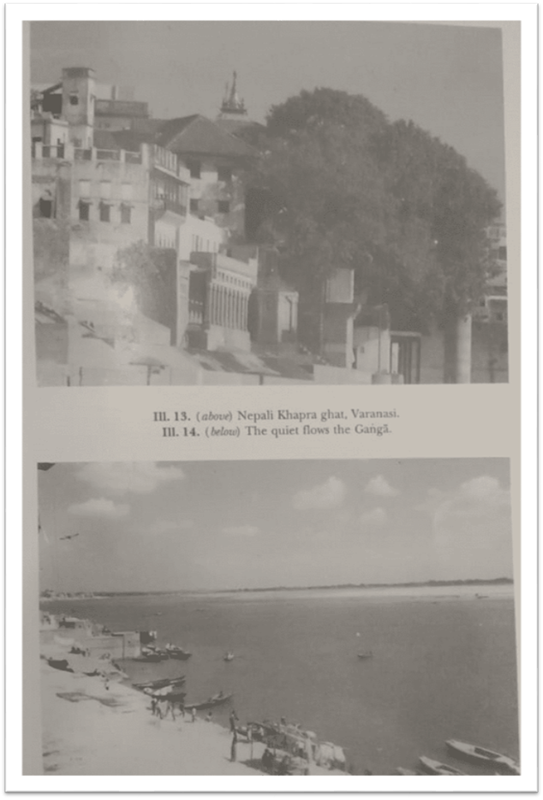
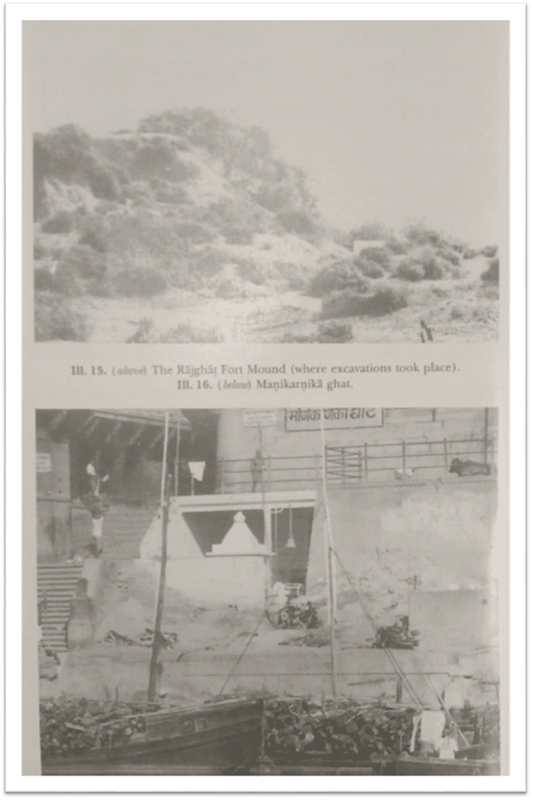
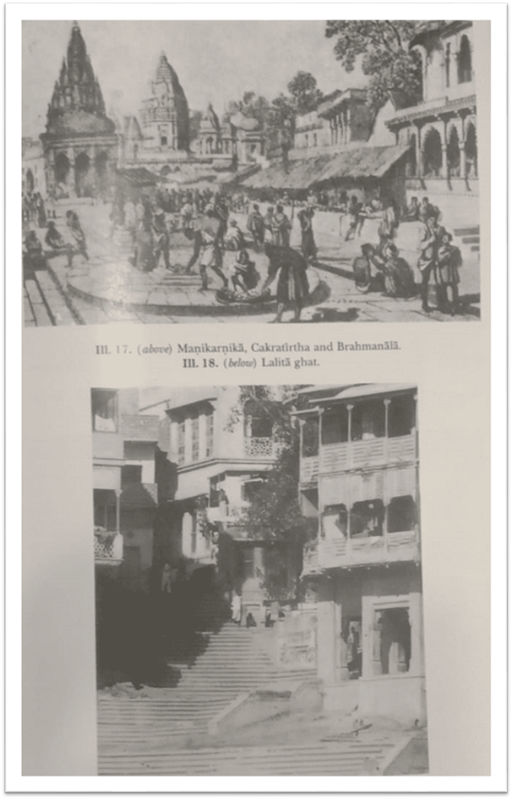
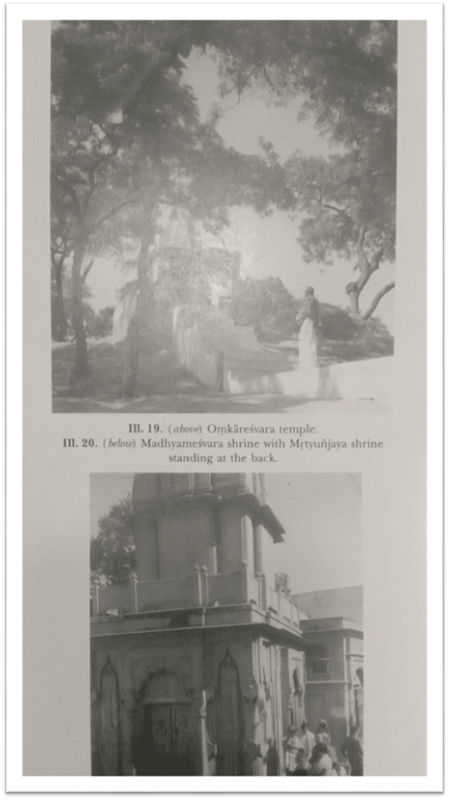
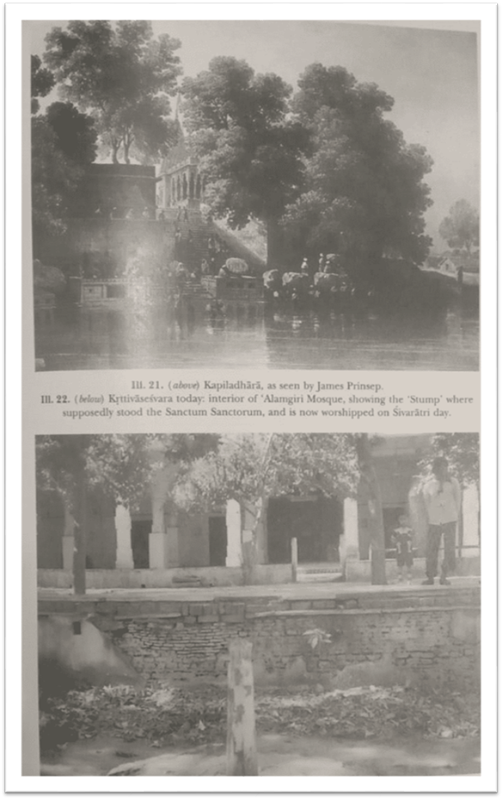
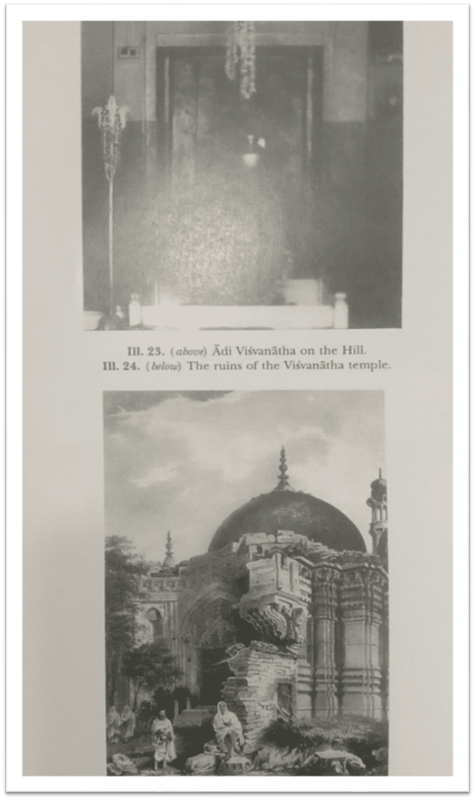
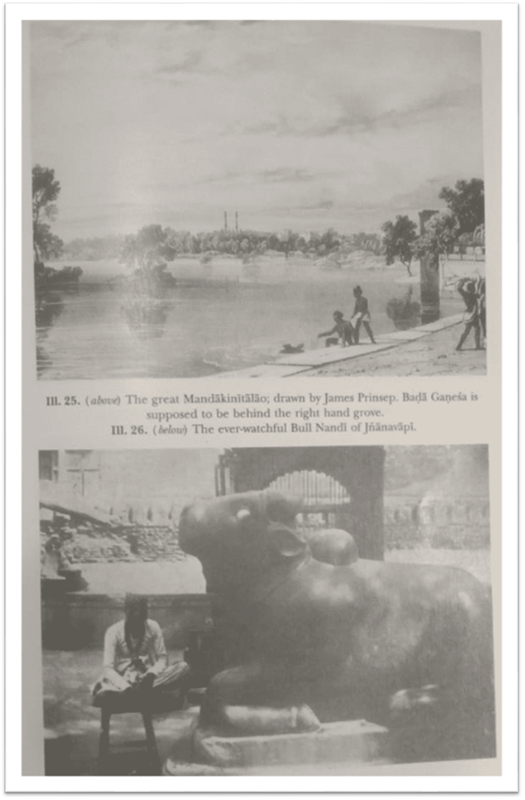
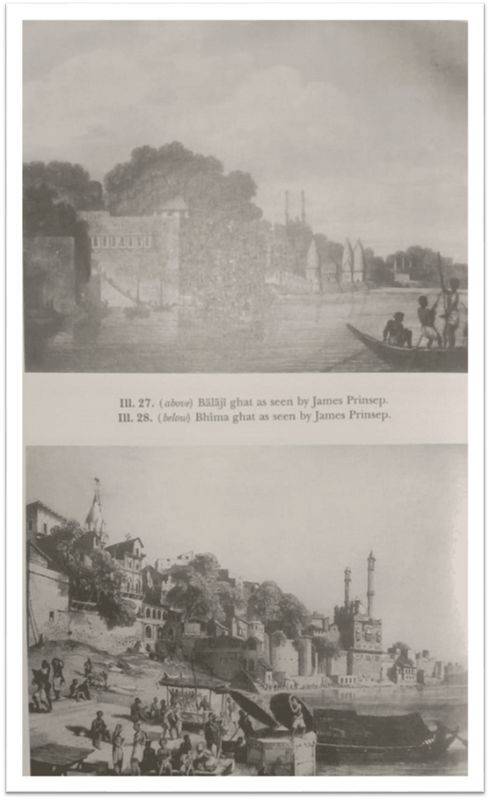

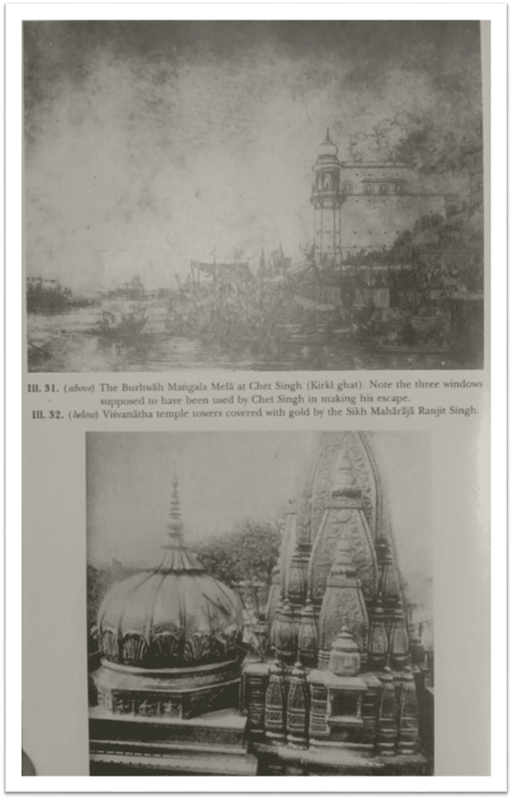
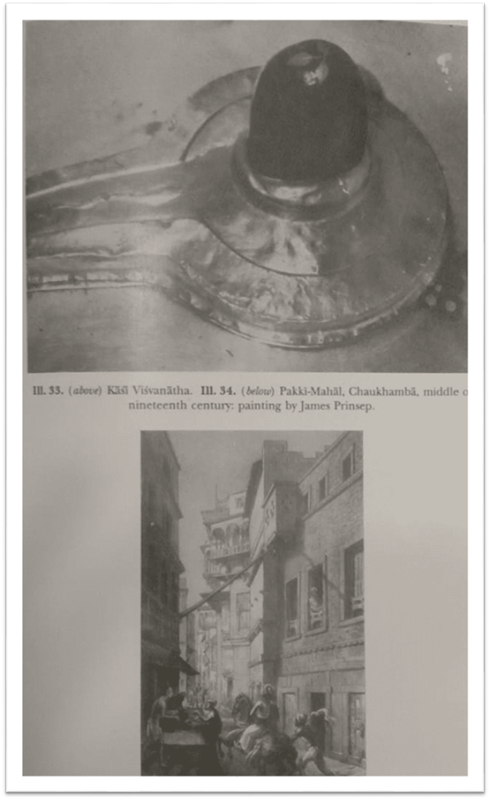
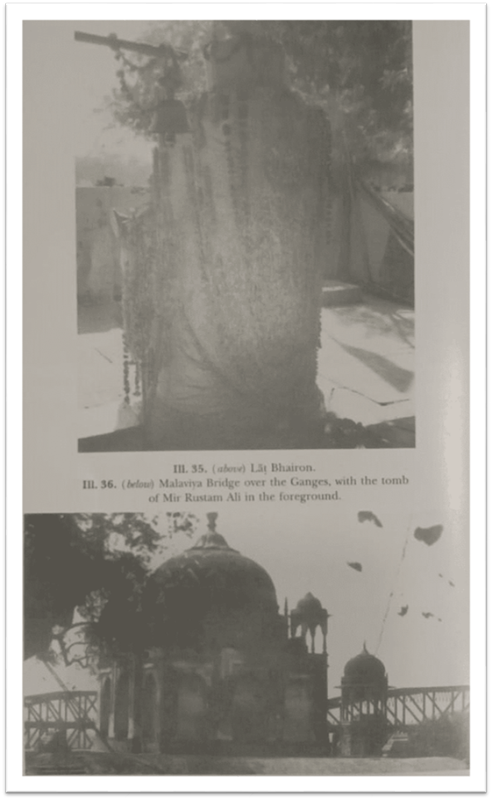
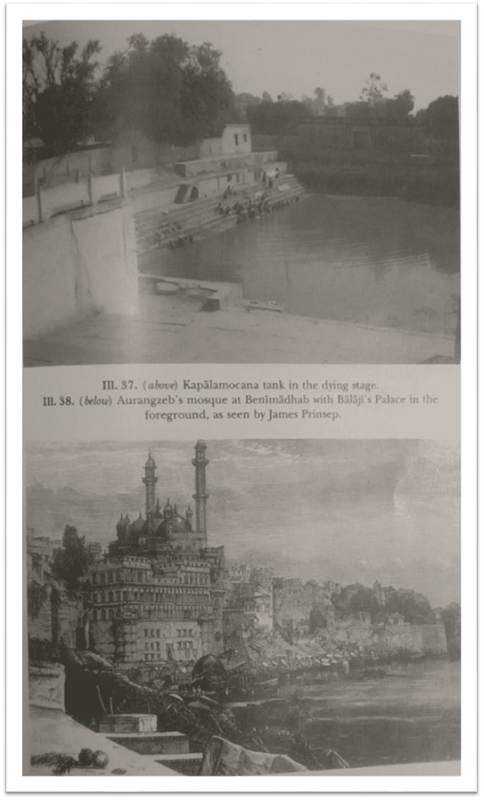
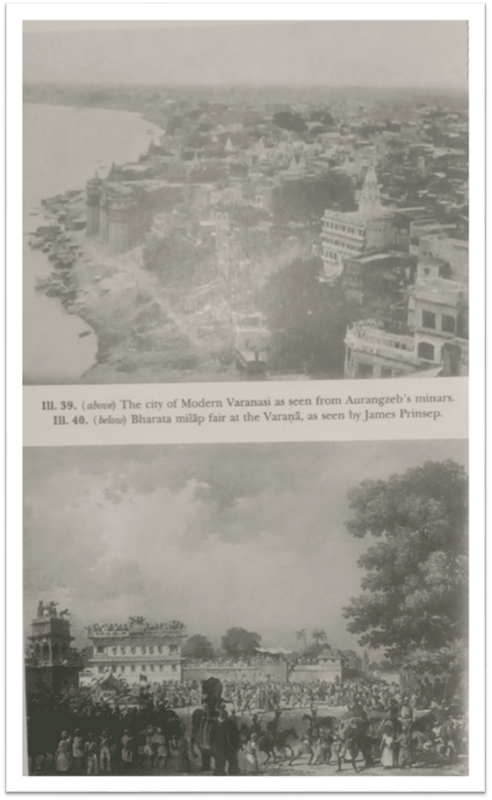
यह संयोग मात्र नहीं था, बल्कि इसके गहरे कारण थे।
खिलजी दक्षिण को तबाह करने में व्यस्त थे और वे इतने अधिक लूट चुके थे कि उन्हें कुछ समय के लिए विराम लेना पड़ा। इसके अलावा, बलबन एक शांतिप्रिय और बुद्धिमान शासक था। उसने अपने अधिकांश हिंदू प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता को समझा।
इसी समय का लाभ उठाकर वाराणसी के हिंदुओं ने मंदिर निर्माण का प्रयास किया। इससे जौनपुर के शर्की सुल्तानों की कट्टरपंथी मानसिकता सतर्क हो गई। उनकी एक राजकुमारी, बेगम रज़िया ने हिंदुओं के भविष्य में पुनर्निर्माण को रोकने के लिए चौदहवीं शताब्दी में 'रज़िया मस्जिद' का निर्माण किया।
संभवतः इसी समय कुछ भक्त हिंदुओं ने लिंगम को सुरक्षित रूप से वर्तमान सत्यनारायण मंदिर के पीछे स्थित पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया।
हम जानते हैं कि एक श्रद्धालु ब्राह्मण ने इस लिंगम को वाराणसी से बाहर ले जाकर सुरक्षित रखा। कुछ समय बाद, यह लिंगम भदैनी क्षेत्र में पुनः प्रकट हुआ, लेकिन इसकी पहचान गुप्त रखी गई।
आज भी यह लिंगम 'आदि विश्वनाथ' के रूप में सम्मानित किया जाता है। इसके लिए एक छोटे मंदिर का निर्माण अकबर के प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल के पुत्र गोवर्धन दास के अनुदान से संभव हुआ।
III
चूँकि वाराणसी में कोई बड़ा मंदिर शेष नहीं था, इसलिए किसी ने भी शहर को क्षति पहुँचाने की परवाह नहीं की। पहाड़ियों के निकट उपेक्षित घाटी में फैले मलबे के ढेर और ज्ञानवापी तालाब के किनारे तक फैली गंदगी ही महान मोक्ष लक्ष्मी-विलास और उसके परिवेश के विगत वैभव के पतन के साक्षी थे। यह स्थल पश्चिम में विस्तृत महान ज्ञानवापी जलाशय के किनारे स्थित था।
लेकिन इन सभी उतार-चढ़ावों की परवाह किए बिना, तीन पर्वत चोटियों की तलहटी से एक शांत नाला बहता हुआ अगस्त्यकुंड (अब गोडौलिया) से मिलता था। यहाँ लक्ष्मीकुंड, मिश्र पोखरा, बेनिया तालाब, सूरजकुंड और महान गोदावरी नाला का जल प्रवाहित होकर एक धारा बनाता था और पूर्व की ओर बहते हुए गंगा से मिल जाता था।
अन्यथा, आज जिस क्षेत्र में बनारसफाटक और ठठेरी बाजार स्थित हैं, वहाँ कभी कबीरचौरा से बेनिया तक घने जंगल हुआ करते थे। चौक थाना और उसके आसपास का क्षेत्र एक दलदली भूमि थी, जिसे बाद में एक चर्च के निर्माण के लिए उपयोग किया गया। सूरजकुंड और लक्ष्मीकुंड से लेकर लक्सा तक का क्षेत्र भी 1890 तक जंगलों से आच्छादित था। गोदावरी नाला, जो अब दशाश्वमेध बाजार और चित्तरंजन पार्क के रूप में जाना जाता है, प्रवाहित होकर प्रयाग घाट पर मुख्य नदी से मिलता था।
यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि इस नदी पर दो पुल मौजूद थे, जिनके नाम आज भी इन स्थानों से जुड़े हुए हैं। एक था 'डेरसी का पुल' और दूसरा 'पुलेर काली' (हिंदी में 'पुल' का अर्थ है पुल)। एक तीसरा पुल गोदावरी धारा पर मारवाड़ी अस्पताल और बड़ा देव के पास था।
जिस क्षेत्र में चौक पहाड़ी स्थित थी, जहाँ मूल मोक्ष लक्ष्मी-विलास मंदिर स्थित था, और पूर्व में वर्तमान ज्ञानवापी और दक्षिण में गोडौलिया तक का क्षेत्र, उसने 500 वर्षों से अधिक समय तक विध्वंस के भयावह दौर देखे हैं। लगातार विनाश के परिणामस्वरूप मलबे के टीले बनते चले गए, जिनकी सफाई एक बड़ी समस्या बन गई।
इस मलबे का एक भाग (1) ज्ञानवापी तालाब में डाला गया, विशेष रूप से औरंगजेब द्वारा अंतिम विध्वंस के बाद, और (2) एक भाग पहाड़ियों के नीचे ढकेल दिया गया, जिससे वर्तमान चौक-गोडौलिया मार्ग बना, जो बनारसफाटक से होकर जाता है। इस मलबे की परतों को आज भी सीढ़ियों की संरचना और एक तीव्र ढलान से पहचाना जा सकता है। सदियों तक यह मलबा बिना हटाए पड़ा रहा।
ज्ञानवापी का जलाशय इस मलबे से भर गया। इसकी याद दिलाने के लिए, आज भी एक संकरी गली मौजूद है, जो चौड़ी सड़क (आधुनिक समय में निर्मित) और दंडपाणि गली से जुड़ती है। इस गली को कटवारखाना (कूड़े का ढेर) कहा जाता है।
सदियों तक चले विध्वंस के कारण, पहाड़ी के पास का क्षेत्र, ज्ञानवापी तालाब तक, मलबे से भर गया। मंदिर परिसर के आसपास के उद्यान अब केवल विस्मृत स्वप्न बन चुके थे। पहाड़ी के चारों ओर पेड़ अपनी नग्नता में खड़े थे, जो एक अपमानित राष्ट्र के शाप को दर्शाते थे। जब ब्रिटिश आए, तो अपने 'गंदे' इलाकों को पुनर्संगठित करने और नगर के केंद्र (चौक कोतवाली) से नदी तक एक मोटर योग्य सड़क बनाने की सुविधा के लिए, उन्होंने पहाड़ी को काटकर एक ढलान बना दिया।
यह ढलान बनारसफाटक से होकर गोडौलिया के समतल भागों को पुराने आदि विश्वनाथ मंदिर की पहाड़ी से जोड़ता है। इसे ज्ञानवापी तालाब से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, सिवाय उन विशाल मलबे के ढेरों के, जो सदियों से जमा हो गए थे और जिन्हें अब आधुनिक निर्माण के तहत हटा दिया गया है, जहाँ एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है।
वर्तमान मंदिर का अस्तित्व केवल मराठाओं के उच्चकाल में संभव हुआ, जब महादजी सिंधिया ने सम्राट शाह आलम से वाराणसी को फिर से हिंदू पवित्र नगर के रूप में स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। इस पर आगे चर्चा करेंगे।
इस मलबे ने पहले ही जलाशय को लगभग भर दिया था। जो कुछ भी तालाब में बचा था, उसे दो चरणों में नष्ट कर दिया गया और भर दिया गया।
हमें याद है कि अकबर और उसके बाद उसके पुत्र जहाँगीर ने खंडित मंदिरों को पुनर्निर्माण की अनुमति दी थी। (जहाँगीर की माता प्रसिद्ध अंबर राजघराने की एक हिंदू राजकुमारी थीं।)
इस शाही स्वीकृति का लाभ उठाते हुए, भारत के हिंदू समाज ने पुनर्निर्माण के कार्य को अत्यंत उत्साह से प्रारंभ किया। इसी समय तालाब के किनारे जमा मलबे का कुछ भाग साफ किया गया और एक नए मंदिर के निर्माण के लिए स्थान बनाया गया। यही वह मंदिर था जिसे गोवर्धनदास ने निर्माण में सहायता प्रदान की।
IV
वर्तमान में रज़िया मस्जिद और आदि विश्वनाथ मंदिर जिस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं, वह चौक क्षेत्र की दक्षिणी सीमा की रक्षा करता है। इस पहाड़ी की ऊँचाई पर एक प्रमुख स्थलचिह्न के रूप में फूल बाजार, सत्यनारायण मंदिर और वर्तमान में कटोरा-बनारसफाटक के नाम से प्रसिद्ध इलाका स्थित है। चौक को गोडौलिया से जोड़ने वाली चौड़ी सार्वजनिक सड़क इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। सड़क के दोनों ओर सजी हुई दुकानें आगंतुक के मन को वास्तविकता से भटका देती हैं।
यदि हम इस सड़क और आधुनिक निर्माणों को अपने मन से हटा दें और उस प्राचीन वैभव की कल्पना करें जो कभी विश्वेश्वर मंदिर और उसके परिसर का हिस्सा था, तो हम अतीत की उस गौरवशाली छवि को पुनर्निर्मित कर सकते हैं।
इस सड़क की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी तीव्र ढलान है, जो दर्शाती है कि यह कभी एक वनाच्छादित पहाड़ी, घाटी और प्रवाहित जलधारा का हिस्सा रही होगी। प्राचीन मानचित्र के अनुसार, बिंदु A से बिंदु B तक भूमि की एकरूप ढलान इंगित करती है कि यह एक घनी वनाच्छादित पहाड़ी थी, जहाँ कभी एक घाटी और प्रवाहित जलधारा थी। बिंदु C पर ज्ञानवापी परिसर स्थित था और बिंदु D पर विशाल अगस्त्यकुंड स्थित था।
यदि हम प्राचीन वाराणसी की भू-संरचना को आनंदकानन की मूल संरचना की तुलना में देखें, तो तीन प्रमुख बिंदु उभरकर सामने आते हैं:
1. आधुनिक विशेष्वरगंज बाजार और कबीरचौरा,
2. गोडौलिया,
3. ज्ञानवापी परिसर।
प्राचीन ग्रंथों में मच्छोदरी का उल्लेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में किया गया है। यह स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों था? मच्छोदरी का अर्थ 'मछली का मध्य भाग' होता है। लेकिन यह मछली क्या थी? इसका स्वरूप कैसा था? क्या यह वाराणसी के मूल भूगोल से जुड़ी कोई संरचना थी?
इस 'मछली संरचना' को समझने के लिए हमें वाराणसी के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के जल मार्गों का पुनर्निर्माण करना होगा। इस क्षेत्र की सीमा वरुणा नदी से लगती है। मच्छोदरी नाला वरुणा को उसी नाम की विस्तृत झील से जोड़ता था। यह झील गंगा की बाढ़ के दौरान जल से भर जाती थी। जब बाढ़ का प्रवाह वरुणा नदी में प्रवेश करता था, तो यह जल को मच्छोदरी जलाशय में भर देता था, जिससे जल स्तर बढ़ जाता और यह जल आगे पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर मंदाकिनी तालाब में मिल जाता।
हम पहले ही इस झील के आकार और महत्त्व की चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक कि जेम्स प्रिंसेप (1820 के दशक) के समय में भी यह झील विशेष्वरगंज से कबीरचौरा तक फैली हुई थी। प्रसिद्ध बड़ा गणेश मंदिर इसके तट पर स्थित था। हमें कल्पना करनी चाहिए कि इस झील का विस्तार डाकघर, टाउन हॉल, कंपनी बाग से लेकर उस उत्तरी सीमा तक था, जहाँ पक्की महल क्षेत्र शुरू होता है।
इस झील में मंदाकिनी नदी का जल प्रवाहित होता था। नारायण दत्त के अनुसार, "इसे मच्छोदरी कहा जाता है क्योंकि यह वाराणसी के मध्य में स्थित था।" यहाँ तक कि काशी खंड भी इसकी पुष्टि करता है। ग्रंथों के अनुसार, इस धारा का जल शिवगणों द्वारा निर्मित एक किले की खाई को भरता था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दो प्रवाहों—गंगा की ऊपरी बाढ़ धारा और एक गुप्त अंतःसलिला धारा—से मिलकर बना था, जिसने आनंदकानन को चारों ओर से घेर लिया था। इस प्रवाह ने प्राचीन काशी को एक 'मछली' के आकार में ढाल दिया था, जिससे इसका नाम 'मच्छोदरी' पड़ा। यह धारा वाराणसी के एक बड़े क्षेत्र को घेरते हुए वरुणा नदी से मिलती थी, जहाँ आज ओंकारेश्वर और कपालमोचन स्थित हैं।
अब, जो लोग कपालमोचन के स्थान से परिचित हैं, वे इस तथ्य को जानकर चकित हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि वरुणा नदी का प्रवाह समय के साथ बदल गया है। फिर भी, कपालमोचन प्राचीन नदी के निकट स्थित है, जबकि ओंकारेश्वर टीले से दूर है।
मच्छोदरी योग को प्राचीन शास्त्रों में बहुत सराहा गया है, लेकिन यह वर्तमान समय में भक्तों को अधिक प्रेरित नहीं करता। प्राचीन काल में गंगा नदी, मच्छोदरी चैनल और मंदाकिनी प्रवाह से वाराणसी पूरी तरह से घिरी हुई थी, जिससे यह विशिष्ट धार्मिक और सामरिक सुरक्षा प्राप्त करता था।
उन दिनों जब यह क्षेत्र ज्यादातर जंगलों से आच्छादित था और केवल वरुणा नदी के किनारे कुछ बस्तियाँ थीं, तो इन जल धाराओं ने मुख्य वाराणसी को पूरी तरह से घेर लिया था और इसे मछली के आकार का बना दिया था। यह तथ्य हमें शहर को एक नई दृष्टि और परिप्रेक्ष्य से देखने का अवसर प्रदान करता है।
जब शास्त्रों में मच्छोदरी योग का उल्लेख किया गया है, और जब काशी क्षेत्र को गंगा द्वारा घेरने की बात की जाती है (जो अब दुर्लभ हो गई है, क्योंकि आधुनिक नगर प्रशासन ने स्थलाकृति को पूरी तरह से बदल दिया है), तो यह स्पष्ट होता है कि उस समय काशी का नगर केवल अंतरगृह क्षेत्र तक ही सीमित था।
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय काशी का मुख्य नगर वरुणा नदी के किनारे बसा हुआ था, जिससे 'वाराणस्य' (बाद में 'वाराणसी') नाम उचित ठहरता है, जिसका अर्थ है 'वरुणा के सामने स्थित नगर'। जब गंगा पूरे नगर को घेर लेती थी और प्रयाग संगम (दशाश्वमेध के निकट) में मुख्य धारा से मिलती थी, तब दक्षिणी वाराणसी, जो आज अपने भव्य मंदिरों और ऊँचे शिखरों के कारण प्रसिद्ध है, अस्तित्व में नहीं थी। यह क्षेत्र बहुत बाद में, शायद अकबर के समय के बाद विकसित हुआ।
इन ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमें उन दिनों की वाराणसी की कल्पना करनी चाहिए। पूरा कबीरचौरा मंदाकिनी के जल से आच्छादित था। तालाब पक्की महल की तलहटी तक फैला हुआ था, जिसमें एक ओर मंदोदरी और दूसरी ओर मच्छोदरी नाला स्थित था। यह क्षेत्र इतना जलमग्न था कि यहाँ नौकाएँ चलती थीं और व्यापारिक वस्तुएँ विशेष्वरगंज और कटरा दीननाथ के प्रसिद्ध बाज़ारों तक लाई जाती थीं। ये बाज़ार आज भी वाराणसी के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में गिने जाते हैं, साथ ही पक्की महल, लक्ष्मी चौबुतरा और नारियल टोला के प्रसिद्ध चाँदी, सोने और रेशम के बाजार भी इसी परंपरा का हिस्सा हैं।
उस समय की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नर्तकियों तथा गणिकाओं का बाज़ार भी इन्हीं इलाकों में स्थित था, जो आज भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल बने हुए हैं।
8.भयावह अत्याचार
I
उपलब्ध सबसे प्राचीन अभिलेखों में वाराणसी को एक ऐसे नगर के रूप में वर्णित किया गया है जो तीन प्रमुख 'पहाड़ियों' के चारों ओर स्थित था। समय के साथ हुए विध्वंस और आधुनिक निर्माणों के कारण आज ये पहाड़ियाँ स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं जा सकतीं, लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्य निर्विवाद है कि प्राचीन वाराणसी वास्तव में इन तीन पहाड़ियों पर और उनके चारों ओर स्थित थी। इन पहाड़ियों के बावजूद, अत्यधिक विनाश के कारण भी इनके अवशेष अब भी मौन साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं।
हमें बस इन मौन साक्ष्यों को पहचानने और उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता है।
पिछले अध्याय में की गई हमारी चर्चा इस तथ्य को और स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए, यह समझाने के लिए कि किसी जलाशय का नाम 'मच्छोदरी' (मछली का उदर) क्यों रखा गया होगा, हमें पूरे वाराणसी नगर क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को समझना पड़ा। वर्तमान समय में इस क्षेत्र की नगर योजना इस ऐतिहासिक संदर्भ को नहीं दर्शाती। यह समझना कठिन हो जाता है कि: (क) एक समय यह क्षेत्र वास्तविक नगर था; (ख) गोडौलिया बिंदु से दक्षिण की ओर का नगर क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन था, केवल भार, भंड, गण, भैरव, यक्ष उपासकों, बीर, कालदेव और गणदेव के भक्तों द्वारा बसाया गया था; (ग) वाराणसी का अधिकांश क्षेत्र, विशेष रूप से वरुणा नदी के दक्षिण में, जल से आच्छादित था; (घ) गंगा नदी पूरे नगर को घेरती थी (वरुणा से कपालमोचन तक) और बेनिया पार्क और लक्ष्मीकुंड के माध्यम से गोदावरी से मिलती थी; (ङ) नगर एक पहाड़ी द्वीप की भांति जलधाराओं से घिरा हुआ था; (च) इस क्षेत्र में अनेक आश्रम, मंदिर और अतिथिशालाएँ विद्यमान रही होंगी।
यदि इन तथ्यों का गहराई से अध्ययन किया जाए, तो वे वाराणसी की प्राचीन नदियों और झीलों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विशेषता को उजागर करते हैं।
प्राचीन वाराणसी की लुप्त नदियों और झीलों के संकेत अभी भी भू-आकृतिक विशेषताओं और स्थान-नामों के माध्यम से खोजे जा सकते हैं। जो भौतिक रूप से विलुप्त हो चुका है, उसे वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्यों की सहायता से फिर से स्थापित किया जा सकता है।
वाराणसी की पुनः खोज में, इन 'लुप्त' नदियों, झीलों और पहाड़ी संरचनाओं के अवशेष हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और हमें ऐतिहासिक नगर संरचना को समझने के लिए उपयोगी दिशानिर्देश प्रदान कर सकते हैं।
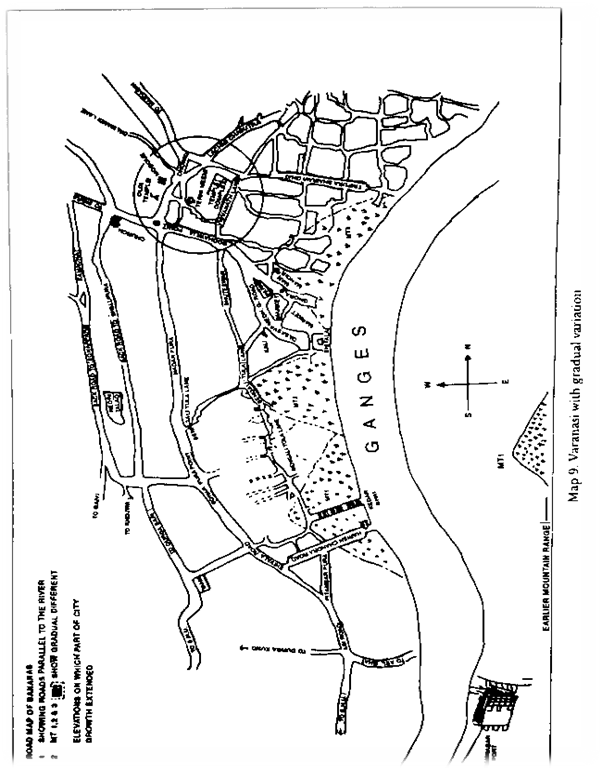
मानचित्र 9. क्रमिक परिवर्तन के साथ वाराणसी
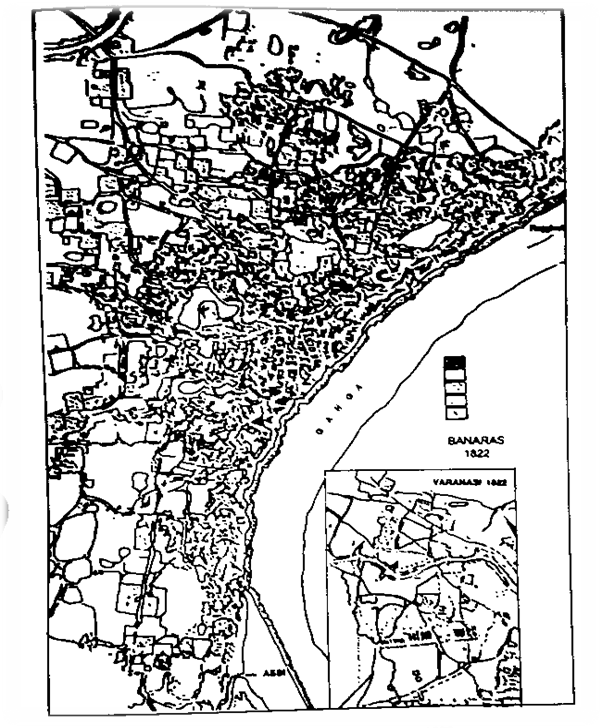
मानचित्र 10. शहर का विकास: बनारस 1822
II
तीन प्राचीन खंडों (खंड) की चर्चा करते समय, सबसे महत्वपूर्ण था केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्र, जिसे अंतरगृह या विश्वेश्वरखंड के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र अब लगभग आदि केशव और दशाश्वमेध के बीच, तथा पश्चिम में कबीरचौरा, राजादरवाजा, बेनिया और गोडौलिया तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र वाराणसी नगर का सबसे ऊँचा स्थान माना जाता है, जिसमें चौक क्षेत्र या विश्वनाथ पहाड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी शामिल है।
आगे चलकर हम जानेंगे कि यह चौक क्षेत्र इतना प्रसिद्ध, भीड़भाड़ वाला और विशिष्ट क्यों बन गया।
यह क्षेत्र प्राचीन वाराणसी की सबसे जटिल और रहस्यमयी तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह इसलिए है क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्षेत्र आनंदकानन की सबसे ऊँची पहाड़ी पर स्थित था। जो स्थान कभी सबसे अधिक एकांत और शांति से भरा हुआ था, वह आज नगर का सबसे व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला हिस्सा बन चुका है। यह परिवर्तन अपने आप में अत्यंत उल्लेखनीय है और इसके पीछे एक लंबी कहानी छिपी हुई है।
यहीं पर महान मंदिर अपने सहायक देवालयों के साथ स्थित था। स्वाभाविक रूप से, यह तीर्थयात्रियों के लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र था। इस्लामी विध्वंस के युगों और इसके परिणामस्वरूप हुए विनाशकारी परिवर्तनों के बावजूद, इस क्षेत्र की लोकप्रियता अब भी बनी हुई है।
इस क्षेत्र में समय-समय पर कई मंदिरों को तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। लेकिन भक्तों की स्मृतियाँ, जैसे किसी प्रिय पालतू की यादें, इन विनाशकारी परिवर्तनों के बावजूद इस स्थान से गहराई से जुड़ी रहीं।
हम अपने प्रियजनों की समाधियों पर जाने की प्रेरणा भी इसी भावना से प्राप्त करते हैं। यदि ऐसे भावनात्मक संबंध न होते, तो येरो की कविताएँ या स्कॉलर जिप्सी जैसी रचनाएँ अस्तित्व में न आतीं। 'प्रिय स्मृतियाँ हमें अतीत की रोशनी से घेर लेती हैं।' स्मृतियों की शक्ति हमारे पूर्वजों की परंपराओं और मूल प्रवृत्तियों को सक्रिय करती है, और बाहरी दबाव इन्हें पूरी तरह मिटाने में असमर्थ रहते हैं।
यह उतार-चढ़ाव सात सौ वर्षों से अधिक समय तक जारी रहे। इन सात सौ वर्षों में क्षय, विनाश और भ्रम ने काशी-वाराणसी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इस दौरान कई विध्वंसों के बावजूद, वाराणसी की जनता अपनी श्रद्धा और आस्था के कारण बार-बार इस पवित्र शिखर, विश्वनाथ शिखर, की ओर आकर्षित होती रही।
जिस प्रकार एक यहूदी यरूशलेम की दीवार की ओर खिंचता है, या एक इस्लामिक भक्त ज़मज़म के जल की ओर आकर्षित होता है, उसी प्रकार वाराणसी के लोग भी हर संकट और विनाश के बाद इस पवित्र स्थल की शरण में आते रहे। अपनी आस्था की ऊष्मा से उन्होंने विध्वंस को पुनर्जन्म में और प्रतिशोध को प्रायश्चित में परिवर्तित कर दिया।
III
आनंदकानन और अविमुक्त क्षेत्र के तपोवन चरण से वाराणसी चरण में परिवर्तन इस्लामी आक्रमण (1194) से कहीं पहले हो चुका था, यहाँ तक कि महान पैगंबर या ईसा मसीह के जन्म से भी पहले। इसके प्रमाण हमें गौतम बुद्ध के काल तक ले जाते हैं। पहले के संघर्षों ने प्राचीन महाश्मशान या रुद्रवास की शांति भंग कर दी थी। मंदिर निर्माण का कार्य शकों के आगमन के बाद आरंभ हुआ, जिसने गण, यक्ष और कपालिकों के वनाच्छादित आनंदकानन को एक ब्राह्मणिक केंद्र में परिवर्तित कर दिया।
आनंदकानन हमेशा से वैदिक अध्ययन का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा था। हम ब्रह्मवास और दशाश्वमेध के पास स्थित ब्रह्मसरोवर के बारे में जानते हैं, जहाँ विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। स्वाभाविक रूप से, बुद्ध इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए, जैसे लोहे को चुम्बक आकर्षित करता है। यदि उन्हें वैदिक परंपरा को चुनौती देनी थी, तो सबसे पहले उन्हें वाराणसी और उसके विद्वानों को प्रभावित करना आवश्यक था। (स्वामी दयानंद ने भी उन्नीसवीं शताब्दी में यही प्रयास किया था।)
हालाँकि, जातक कथाओं के अनुसार, बुद्ध वाराणसी आए थे, आनंदकानन नहीं। इस क्षेत्र को हैहय और प्रतिहारों के बीच हुए संघर्षों ने और अधिक क्षतिग्रस्त कर दिया था। इन संघर्षों की गूँज वेदों और काशी खंड में सुनाई देती है। इन संघर्षों को 'गणों' (स्थानीय समुदायों) और प्रवासी आर्यों के बीच की अशांति के रूप में भी जाना जाता है।
वाराणसी में बिखरे वीर स्मारकों की श्रृंखला आर्य-गण संघर्षों की याद दिलाती है। भैरव, कपाल, यक्ष, या गणपति के मंदिर इन रक्तरंजित युद्धों की समाप्ति के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। ये स्मारक साक्षी हैं कि कैसे शिव के अनुयायियों ने वेदिक प्रभाव के आगे आत्मसमर्पण करने से इनकार किया और अंततः समझौते हुए।
हमने पहले ही वाराणसी को घेरने वाले गण-नायकों और उनके मंदिरों की चर्चा की है। भैरव मंदिरों का उल्लेख भी किया गया है। वीर, कपाल, यक्ष और देव मंदिर इससे भी अधिक प्राचीन हैं।
उन्हीं भयावह संघर्षों के समय से लेकर आज तक, हिंदू किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत बिना इस समझौते को याद किए नहीं करते। भैरव, वीर और गणपति को पहले पूजा जाता है। हिंदू धर्म में गणेश या गणनायक, जो गणों के स्वामी हैं, को सभी अनुष्ठानों में प्राथमिकता दी जाती है।
इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैदिक आक्रमणकारियों ने अविमुक्त क्षेत्र (वह घाटी जहाँ से शिव कभी प्रस्थान नहीं करते) पर अपना अधिकार स्थापित करने से पहले, स्थानीय देवताओं—भैरव (तांत्रिक शिव) और उनके अनुचरों को स्वीकार कर लिया था। इन्हीं शक्तिशाली रक्षकों के संरक्षण में शिव अपनी शक्तियों के साथ रहस्यपूर्ण सान्निध्य बनाए रखते थे। विश्वनाथ स्वयं भैरव का ही रूप हैं। (विशालाक्षी उनकी अर्धांगिनी हैं, जैसे वज्रयान परंपरा में यमान्तक और तारा का संयोग)।
इसका मूल तथ्य यह है कि संघर्षों और विध्वंसों के बावजूद, आनंदकानन का पूर्व-वैदिक स्वरूप अपरिवर्तित बना रहा और वर्तमान अर्धचंद्राकार नगर आज भी वैदिक और गैर-वैदिक सभी हिंदू परंपराओं के मिलनस्थल के रूप में खड़ा है।
गण-काल से देव-काल में परिवर्तन में कई शताब्दियाँ लगीं, जब तक कि दिवोदास और प्रतर्दन का समय नहीं आया। इस प्रकार, गण-शिव और रुद्र-शिव की भूमि आनंदकानन का रूपांतरण वाराणसी में हुआ, जो पहले रुद्रवास के रूप में विख्यात था।
बाद में, इस पर हिंदू शासकों जैसे अजातशत्रु (ईसा पूर्व चौदहवीं शताब्दी) द्वारा भारी विध्वंस किया गया। संभवतः इसी समय वाराणसी का नाम काशी में परिवर्तित हुआ। हैहय और कलचुरी राजाओं के आक्रमणों ने, जैसा कि हम जानते हैं, गहड़वालों को अपनी राजधानी को वरुणा नदी के दक्षिण में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया (दसवीं शताब्दी ईस्वी)।
इस प्रकार, आनंदकानन औपचारिक रूप से वाराणसी बन गया। यह वन्य क्षेत्र अब एक शहरी नाम से जाना जाने लगा। इस नाम की लोकप्रियता ने इतिहास में एक वाराणसी के बजाय चार वाराणसियों के अस्तित्व को स्थापित कर दिया।
इन सभी विध्वंसों, वेद-गण-बौद्ध संघर्षों के बाद, अफगानों द्वारा किए गए आक्रमण सबसे अधिक विनाशकारी सिद्ध हुए। इन आक्रमणों ने वाराणसी को कई बार धूल में मिलाया और पुनः उठने के लिए मजबूर किया, लेकिन एक बदले हुए स्वरूप में। यह एक पूर्ण कायाकल्प की गाथा है।
यदि हम इन विध्वंसों को संचित मलबे के वास्तविक भार में मापें, तो पाएंगे कि इस मलबे का अधिकांश भाग उस केंद्रीय पहाड़ी पर केंद्रित था, जहाँ प्राचीन विश्वनाथ मंदिर स्थित था। यह मलबा बार-बार हटाया गया और शहर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया।
हमारा कार्य कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि हमें आनंदकानन या वाराणसी को काशी खंड, फाह्यान और ह्वेनसांग के विवरणों के अनुसार पुनः संरचित करना होगा।
प्राचीन नदियाँ, झीलें और तालाब, जिन्हें कभी पवित्र माना जाता था, अब पहचान से परे नष्ट कर दिए गए हैं। विभिन्न युगों में विध्वंसक शक्तियों ने अपनी विनाशलीला के दौरान उत्पन्न मलबे को झीलों और नदियों में फेंक दिया, या उन्हें यूँ ही छोड़ दिया।
उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके कार्यों से मनुष्य जल जैसी आवश्यक वस्तु से वंचित हो सकता है या वे किसी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास के प्राकृतिक प्रमाणों को स्थायी रूप से मिटा सकते हैं। (ये जघन्य कार्य 1991 तक भी जारी रहे, जब सरकार की उपेक्षा के कारण वाराणसी को अतिक्रमण करने वाले भू-माफियाओं द्वारा नष्ट किया गया।)
इन नदियों, झीलों और जलमार्गों के नष्ट होने से उन घाटियों की सुंदरता, संतुलन और शांति हमेशा के लिए समाप्त हो गई, जो कभी तीन पहाड़ियों के बीच प्रसिद्ध थीं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कार्यों ने समय के साथ कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाणों को भी मिटा दिया। (लेखक स्वयं सूरजकुंड और बकरीयाकुंड के विनाश का साक्षी रहा है। अब महान ईसरगंग तालाब को 'हमला' झेलना पड़ा। यह सब हिंदुओं द्वारा ही किया गया।)
इसी तरह की अविवेकपूर्ण हरकतों के कारण आनंदकानन नामक यह सुंदर तपोवन हमेशा के लिए नष्ट हो गया। इसकी प्राकृतिक शांति और आध्यात्मिकता पहले काशी और मगध (ईसा पूर्व 1840-1484) के राजाओं के संघर्षों से, फिर काशी और कोशल (644-1194) के संघर्षों से समाप्त हो गई।
इन संघर्षों ने काशी के शासकों को अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया, जो गहड़वालों के समय (1094) में हुआ। शहर वरुणा नदी के प्राचीन तट से फैलकर पंचगंगा पहाड़ियों तक और मच्छोदरी तथा गंगा के किनारों तक विस्तृत हो गया।
इसके बावजूद, वास्तविक क्षति सीमित रही। आनंदकानन का हृदय और आत्मा, जो अभी भी नगर के दक्षिण में संकटा मोचन तक विस्तृत था, 1910 तक अपनी विशेषताओं को बनाए रखा।
IV
भौगोलिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित हो चुका है कि प्राचीन वाराणसी का मूल क्षेत्र वर्तमान राजघाट क्षेत्र था। यह क्षेत्र मच्छोदरी और मंदाकिनी तालाब (तड़ाग) के किनारों तक विस्तृत था। गहड़वाल अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि गहड़वाल राजाओं (जिन्होंने किला बनवाया) को वरुणा संगम पर स्थित आदि केशव घाट पर स्नान करना अत्यंत प्रिय था।
मच्छोदरी जलधारा (मंदाकिनी के माध्यम से) गंगा से नौकाओं और बड़े जहाजों को नगर के विशाल बाज़ार तक सीधे लाने की सुविधा प्रदान करती थी।
कई विध्वंसों के बावजूद, आनंदकानन का हृदय क्षेत्र काफी हद तक सुरक्षित बना रहा। काशी राज्य, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वनाच्छादित आनंदकानन के साथ सह-अस्तित्व में रहा। हालाँकि, वाणिज्यिक और सांसारिक जनसंख्या के अचानक प्रवाह ने इस वनस्थलीय निवास की प्रकृति और माहौल को बदल दिया। ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी तक आनंदकानन की हरितिमा लगभग अपरिवर्तित बनी रही।
अफगानों और अफरीदियों के लगातार आक्रमणों के बाद तुगलक, खिलजी और लोदी शासकों के आक्रमणों (1194-1660) ने आनंदकानन के शांत जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।
पहले मुक्त लुटेरों की लालच और फिर श्वेत साम्राज्यवादियों की ठंडी, निर्दयी नीतियों ने वाराणसी के शेष बचे स्वरूप को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वास्तविक वाराणसी और आनंदकानन को इस लालच और उन स्वघोषित 'नगर-नायकों' की मिलीभगत ने ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने इसके संरक्षण का दायित्व लिया था।
धर्म, व्यापार या सीधी निष्ठुरता के नाम पर प्रकृति की संपदा से छेड़छाड़ करना इतिहास और संस्कृति के प्रति सबसे घोर अपराध है। पर्यावरण की ताजगी प्रकृति का वरदान है। मनुष्य इसे नष्ट कर सकता है, लेकिन वह इसे पुनः निर्मित नहीं कर सकता।
आश्चर्य नहीं कि आज का जिज्ञासु इन अंतर्देशीय जल स्रोतों के अवशेषों को लेकर भ्रमित महसूस करता है। जैन-बौद्ध ग्रंथों, पुराणों और विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार, इन जल स्रोतों ने प्राचीन आनंदकानन और ऐतिहासिक वाराणसी को समृद्ध बनाया था।
आज की वाराणसी में वह स्थलाकृतिक संकेत कहीं नहीं मिलते, जिनका उल्लेख काशी खंड और बाद के ऐतिहासिक अभिलेखों तथा विदेशी यात्रियों के विवरणों में किया गया था।
V
यहाँ मोक्ष लक्ष्मी-विलास मंदिर की भव्यता का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जैसा कि ह्वेनसांग ने वर्णन किया है।
उनके विवरण के अनुसार, उनके समय (ईसा पश्चात 643) में वाराणसी में लगभग सौ प्रमुख और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर थे। इनमें मोक्ष लक्ष्मी-विलास मंदिर सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा था। इसके स्वर्णिम शिखर का दृश्य वरुणा नदी के उत्तरी तट से बहुत दूर से भी देखा जा सकता था।
ह्वेनसांग ने वाराणसी के आसपास लगभग बीस बौद्ध विहारों की उपस्थिति का भी उल्लेख किया है, हालाँकि स्वयं नगर में कोई बड़ा विहार नहीं था, सिवाय एक के, जो मुख्य मंदिर, मोक्ष लक्ष्मी-विलास के निकट स्थित था।
वर्तमान में भी महान मस्जिद में उपलब्ध सामग्री इस ऐतिहासिक प्रमाण की पुष्टि करती है। पुरातत्वविदों ने पाया है कि मस्जिद के निर्माण में प्रयुक्त स्तंभ, रेलिंग, मेहराब, कोने की पकड़ और खंभे निर्विवाद रूप से जैन और बौद्ध स्थापत्य परंपराओं से संबंधित हैं।
जो भी हो, वर्तमान वाराणसी में अब कोई अन्य बौद्ध निर्माण नहीं बचा है। केवल सारनाथ इसका एक अपवाद है। आधुनिक काल तक, प्रसिद्ध बौद्ध परिसर के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सारनाथ की खोज संयोगवश हुई, जब रेलवे लाइन बिछाते समय एक इंजीनियर को ये रहस्यमयी अवशेष दिखाई दिए। सौभाग्य से, भारतीय पुरातत्व विभाग ने इन अवशेषों को संरक्षित किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजघाट के अवशेषों को समय पर बचाया नहीं जा सका।
लेकिन क्या वास्तव में सारनाथ वाराणसी से इतना दूर था? या फिर वाराणसी के उत्तरी भाग को एक के बाद एक आक्रमणों ने मिटा दिया? तब वाराणसी वास्तव में कहाँ स्थित थी?
सारनाथ, जो आधुनिक (गहड़वालों के बाद की) वाराणसी की सीमा के बाहर और वरुणा नदी के पार स्थित है, ने एक विशाल बौद्ध परिसर को उजागर किया है। जातक कथाओं के अनुसार, गौतम बुद्ध ने वाराणसी में अपना पहला उपदेश (530 ईसा पूर्व) दिया था। वास्तव में, वे लंबे समय तक सारनाथ में रहे थे। यह प्रमाणित करता है कि वाराणसी, जो काशी की राजधानी थी, वरुणा नदी के दोनों किनारों पर स्थित थी।
महान चीनी यात्री ने वाराणसी और इसके मंदिरों की सुंदरता का अत्यंत भावनात्मक वर्णन किया है।
उन्होंने मंदिर को एक विशाल उद्यान के केंद्र में स्थित बताया, जो पक्के पथों से सुरक्षित था। वे विशेष रूप से विशाल मंदिर प्रांगणों का उल्लेख करते हैं, जो महंगे और चमकदार पत्थरों से ढके हुए थे। दीवारों को पत्थर की सुंदर नक्काशीदार मूर्तियों से सजाया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी वर्णन की गई वाराणसी वह क्षेत्र था जो उत्तर में वरुणा नदी से दक्षिण में विश्वनाथ पहाड़ी तक फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान विशेश्वरगंज, पक्की महाल, कुँजीटोला और दलमंडी के बाजार शामिल थे।
उनके विवरणों में सबसे उल्लेखनीय था शिव की विशाल प्रतिमा, जो ठोस तांबे से बनी थी और ध्यानमग्न योगी के रूप में थी। इसकी ऊँचाई 66 हाथ (लगभग 100 फीट) थी! इतनी बड़ी मात्रा में तांबे की यह मूर्ति किसी भी लालची अफगान आक्रमणकारी के लिए लूट का प्रमुख लक्ष्य हो सकती थी।
यात्रियों के विवरणों के अलावा, हमारे पास पुराणों के प्रमाण भी हैं, जिनमें स्कंद पुराण का काशी खंड सबसे महत्वपूर्ण है। वायु पुराण और अग्नि पुराण भी सहायक हैं। यदि हमें वाराणसी के अतीत पर ठोस निष्कर्ष निकालने हैं, तो काशी खंड और काशी महात्म्य के प्रमाणों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
हमें काशी खंड को केवल एक कल्पना मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। पुराण आमतौर पर समय की लोकप्रिय मान्यताओं, परंपराओं और संदेशों को दर्ज करते हैं। वे नई कहानियाँ गढ़ते नहीं हैं।
हम वाराणसी के गुम हुए स्वरूप को पुनः खोजने का प्रयास करेंगे, जिसमें तीन पहाड़ियों के अवशेषों की सहायता ली जाएगी। इसी कारण काशी को शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ कहा गया है। ये तीन पहाड़ियाँ वास्तव में त्रिशूल जैसी प्रतीत होती हैं और यह पुष्टि करती हैं कि 'काशी अन्य सभी मानव बस्तियों से अलग और श्रेष्ठ थी।'
कैरेबियाई सागर में तीन पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण कोलंबस ने उस स्थान को त्रिनिदाद नाम दिया था। विश्वभर में ऐसे कई त्रिनिदाद हैं। स्थानों के नामकरण में भौगोलिक विशेषताओं को आधार बनाना एक सामान्य प्रथा रही है।
हमने पहले ही उल्लेख किया है कि वाराणसी का सबसे ऊँचा बिंदु चौक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जौनपुर के शर्की वंश की रज़िया बेगम (लगभग 1473) की मस्जिद स्थित है।
मस्जिद के ठीक निकट, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, वह छोटा सा मंदिर स्थित है जिसे गोवर्धनदास ने बनवाया था और जिसमें आदि विश्वनाथ की स्थापना की गई थी। यह वही स्थल हो सकता है जहाँ चीनी यात्री द्वारा वर्णित मूल मोक्ष लक्ष्मी-विलास मंदिर स्थित था।
आज यह स्थल एक घनी आबादी वाले व्यावसायिक केंद्र में तब्दील हो चुका है, जो अत्यंत अशोभनीय प्रतीत होता है। लेकिन जब यहाँ कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं थे, जब यहाँ दुर्गंधयुक्त गलियाँ नहीं थीं, जब पहाड़ियों की ढलानें धीरे-धीरे ज्ञानवापी के जल से मिलती थीं, तब इस मंदिर परिसर की भव्यता और हरियाली की पृष्ठभूमि वास्तव में अविस्मरणीय रही होगी।
इसी स्थान पर चीनी विद्वान ने मंदिर को अपनी संपूर्ण भव्यता में देखा था। उन्होंने सुव्यवस्थित उद्यानों, धर्मशालाओं, विश्राम गृहों, मंदिर के कर्मचारियों के निवास स्थान, संगीतज्ञों, सुंदर देवदासियों, हाथी-घोड़ों के अस्तबलों, झरनों और सरोवरों से सुसज्जित इस भव्य परिसर का उल्लेख किया था।
ऐसे मंदिर परिसर दुनिया भर में विद्यमान रहे हैं, जैसे कि अंकोरवाट, अंकोरथोम, बोरोबुदुर, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, रामेश्वरम, श्रीरंगम, त्रिवेंद्रम, बेल्लूर, हलिबिड, हम्पी और अन्य। ये हमें बाबुल, उर, पर्सेपोलिस और फिलिस्तीन के विशाल मंदिर परिसरों की याद दिलाते हैं।
यह क्षेत्र वाराणसी का सबसे ऊँचा स्थान भी था। जब चीनी यात्री ने इस ऊँचे स्वर्णिम शिखर के मंदिर की सुंदरता का वर्णन किया, तो निस्संदेह वह इसी मंदिर की बात कर रहे थे। यही वह मंदिर था जिसे अफगानों द्वारा बार-बार ध्वस्त किया गया।
वाराणसी के मंदिरों की अपार संपत्ति ने उन्हें आक्रमणकारियों के लिए आकर्षक लक्ष्य बना दिया।
यह कल्पना करना कठिन नहीं कि वाराणसी के प्रमुख मंदिरों की संपत्ति अत्यंत विशाल रही होगी, विशेष रूप से एक सौ फीट ऊँची ठोस तांबे की मूर्ति को देखते हुए। ओंकारेश्वर, कृतिवासेश्वर, अविमुक्तेश्वर, कालेश्वर, मध्यमेंश्वर और दंष्ठहस्तेश्वर के मंदिरों सहित, वाराणसी के मंदिरों की संपत्ति इतनी विशाल थी कि इसे लूटने का लालच अफगान और फारसी आक्रमणकारियों को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता था।
VI
आइए, अब मंदिर क्षेत्र और उसके परिवेश का विस्तार से अध्ययन करें। आज यह क्षेत्र चौक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आधी सदी पहले इसे नया चौक कहा जाता था। चौक का अर्थ होता है 'नगर का मुख्य केंद्र' या व्यापारिक स्थल। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पहाड़ी के सर्वोच्च भाग का महत्व यहाँ स्थित प्रमुख मंदिर के कारण ही था। व्यापार और वाणिज्य का केंद्र स्वाभाविक रूप से मंदिर के चारों ओर विकसित हुआ। ज्ञानवापी से मच्छोदरी तक, पहाड़ी की ढलानों पर व्यापार फला-फूला, तब भी और आज भी।
लेकिन इसे 'नया' चौक क्यों कहा गया?
'चौक' शब्द एक हिंदू नगर व्यवस्था से संबंधित है। 'पुराना' चौक निश्चित रूप से मंदिर परिसर के निकट स्थित रहा होगा, जिसे लूट के उद्देश्य से किए गए आक्रमणों में नष्ट कर दिया गया।
वाराणसी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, जिसके लिए एक केंद्रीय बाज़ार आवश्यक था। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे एक व्यवस्थित बाजार क्षेत्र के रूप में विकसित किया, जिसे 'नया चौक' कहा जाने लगा। विशेष रूप से 1857 के बाद, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहाँ पुलिस मुख्यालय का निर्माण किया गया।
नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एक सड़क राजघाट रेलवे स्टेशन से लेकर दशाश्वमेध तक बनाई गई, जो गोडौलिया से होकर गुज़री। यह सड़क पुराने मंदिर क्षेत्र से होकर गुज़री, जहाँ सदियों से जमा मलबे को हटाना पड़ा। इसके निर्माण में मंदाकिनी तालाब, ज्ञानवापी और गोदावरी तालाब बाधा थे। सबसे सरल समाधान था कि झीलों और नदियों को भर दिया जाए। सदियों से जमा मलबे का उपयोग करते हुए इन जल स्रोतों को समाप्त कर सड़क बना दी गई।
ब्रिटिश प्रशासन के लिए 'पुलिस' प्रमुख शक्ति का प्रतीक थी। वाराणसी में पुलिस मुख्यालय के लिए इस प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र से बेहतर स्थान नहीं हो सकता था, जहाँ महान मंदिर स्थित था। पूरे क्षेत्र को ध्वस्त कर, संकरी गलियों और अवैध गतिविधियों को हटाकर नया चौक बनाया गया, जहाँ पुलिस मुख्यालय प्रमुख बना। पुरानी मुस्लिम अदालत भी पास में स्थित थी। आज भी 'पुराना चौक' के रूप में एक क्षेत्र जाना जाता है।
पुनर्निर्माण को नया स्वरूप देने के लिए पूर्वी ओर आधुनिक वास्तुकला की दो मंजिला इमारतें बनाई गईं और कचौड़ी गली के पास एक विशाल मेहराब द्वारा इसे सीमित किया गया।
पश्चिमी भाग को छोड़ दिया गया। यहाँ पुराने गलियों को नहीं बदला गया, और यह क्षेत्र वाराणसी का वेश्यालय क्षेत्र बना रहा।
लेखक, जो 1910 में वाराणसी में जन्मे और पले-बढ़े, इस अनूठे शहरी ढांचे को लेकर सदैव प्रश्न करते रहे हैं। मंदिर परिसर के निकट ऐसी दुकानों और अनैतिक गतिविधियों की उपस्थिति क्यों थी? यहाँ अधिकांश व्यापारी मुस्लिम क्यों थे? और वे विदेशी चमकीले सामान, शीशे, कंघे, इत्र, खिलौने आदि क्यों बेचते थे?
सामाजिक संरचना के अनुसार, इस क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों का वर्चस्व होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। दलमंडी से लेकर बेनिया और कुदाई चौकी तक यह क्षेत्र मुस्लिम आबादी से भरा हुआ था। ये लोग उच्च कुलीन मुस्लिम समाज से नहीं थे, बल्कि कारीगर थे, जो अपने प्राचीन शिल्प में निपुण थे।
VII
विदेशी आक्रमणों ने इनके शांत जीवन को तहस-नहस कर दिया। धर्मांतरण से व्यक्ति की आत्मा बदल सकती है, लेकिन उसकी पारंपरिक कला और जीविका के साधन अपरिवर्तित रहते हैं। वाराणसी के शिल्प कौशल की प्रशंसा महाकाव्यों और जातक कथाओं में की गई है।
मजबूरी में धर्मांतरण से किसी भी समुदाय के गौरव में वृद्धि नहीं होती। इसके विपरीत, यह आंतरिक विद्रोह और कट्टरता को जन्म देता है। इतिहास बताता है कि जबरन धर्म परिवर्तन झेलने वाले समाजों ने क्रूर अत्याचारियों को जन्म दिया है, जिन्होंने बदले की भावना से रक्तपात किया।
धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अपने पारंपरिक समुदाय से अलग हो जाता है, लेकिन उसकी जीविका का साधन वही रहता है।
आज भी जयपुर में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाने वाले अधिकांश मूर्तिकार मुस्लिम हैं। परंपरागत व्यवसाय में गहरी आस्था ही सभ्यता के विकास का आधार रही है।
आजीविका का प्रश्न धर्म परिवर्तन की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस सच्चाई का सबसे स्पष्ट उदाहरण वाराणसी के मुस्लिम कारीगरों में देखा जा सकता है।
हालाँकि, यह भी सत्य है कि इस परिवर्तित समुदाय को एक अत्यंत परिष्कृत फ़ारसी संस्कृति का प्रभाव मिला, जिसे लखनऊ के नवाबों ने संरक्षित किया।
वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध हस्तकला का श्रेय मिश्रित हिंदू-मुस्लिम समाज को जाता है। राजनीतिक रूप से प्रेरित सांप्रदायिक तनाव के बावजूद, वाराणसी के कारीगरों का परस्पर सहयोग और सौहार्द्र प्रशंसनीय है। यह कारीगर समुदाय और व्यापारिक संघ की मजबूत एकता सामाजिक-आर्थिक विशेषज्ञों को भी चकित कर सकती है।
VIII
इस संदर्भ
में केवल विदेशी आक्रमणों को
ही वाराणसी के विनाश के
लिए दोषी ठहराना ऐतिहासिक रूप
से निरर्थक है।
पूर्व-मुस्लिम काल के अभिलेख
इतिहासकारों को
यह कहने के लिए प्रेरित
नहीं करते कि जैन, बौद्ध या हिंदू राजाओं—जैसे प्रतिहार और
गहड़वाल (प्रसेनजित और अजातशत्रु)—ने ऐसा नहीं किया।
जब भी उन्हें अवसर मिला,
उन्होंने आक्रमण किया,
विध्वंस किया, यहाँ तक कि
धर्मांतरण भी कराए। वे यह
नहीं समझ सके कि सामाजिक
संस्थाओं का विनाश ऐतिहासिक पहचान
का विनाश होता है।
और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह मानव संसाधन का विनाश भी होता है। सदियों से संचित धन की अंधाधुंध लूट से लुटेरे कम पीड़ित होते हैं, लेकिन जिनका धन लूटा जाता है, वे आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। उनकी आत्म-सम्मान की भावना और राष्ट्रीय गौरव पर गहरी चोट लगती है। उनका मानसिक संतुलन हिल जाता है और इसके कारण राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इस प्रकार के पागलपन भरे आक्रमण मानव में मानव के प्रति विश्वास को समाप्त कर देते हैं। आध्यात्मिक क्षति की भरपाई करने के लिए लोग धीरे-धीरे कट्टरता की ओर बढ़ते हैं। किसी संस्कृति की आत्मा, उसी तरह जैसे मानव आत्मा, विध्वंस की तीव्रता से स्थायी रूप से विक्षिप्त हो जाती है। यूरोप में यहूदियों के प्रति द्वेष इसका एक उदाहरण है। तथाकथित धार्मिक युद्ध वास्तव में सत्ता और लूट, आर्थिक लाभ और व्यापारिक हितों के लिए लड़े गए युद्ध माने जा सकते हैं। धर्म केवल एक पवित्र मुखौटा प्रदान करता है, जिससे दुष्टों और हत्यारों को अपने असली चेहरे छिपाने में सुविधा होती है।
धर्म का उपयोग अक्सर अनैतिक रूप से संपत्ति और सत्ता हासिल करने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन ऐसे आक्रमणों के पीछे वास्तविक प्रेरणा मनुष्य की असीमित सत्ता और धन की लालसा रही है। इस दृष्टि से, भारत कभी भी गरीब और दबे-कुचले वर्ग के लिए शांतिपूर्ण स्थान नहीं रहा, जो सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के शोषित वर्ग थे। उनके लिए शांति का अर्थ था मूक पीड़ा और कुंठा को चुपचाप सहन करना। इस संदर्भ में हिंदू भी अपवाद नहीं थे, क्योंकि वे भी मनुष्य ही थे। उन्होंने भी अपने धार्मिक युद्ध लड़े—चाहे वह शैव-वैष्णव संघर्ष हों, ब्राह्मण-गण प्रतिद्वंद्विता हो या फिर बौद्ध और तांत्रिक संघर्ष।
हिंदू राजनीतिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया। इन व्यवस्थाओं में शासकों को नियमित रूप से कमजोर राज्यों पर आक्रमण कर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निर्देश दिया गया था। (मनु और मैकियावेली इस संदर्भ में अलग नहीं थे।) उन्हें अपनी सेनाओं को हर समय तैयार रखने और यदि आवश्यक हो तो मौसमी आक्रमण करने की परंपरा का पालन करने को कहा गया था, जो लगभग एक अनुष्ठान बन चुका था। हिंदू राजनीति ने इसे स्वीकार किया, और हिंदू वीरता ने इसे प्रमाणित किया। (शुक्रनीति, अर्थशास्त्र, महाभारत का शांतिपर्व)।
इसी उद्देश्य से वर्ष के एक विशेष दिन (आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी) को युद्ध की देवी महिषासुरमर्दिनी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित किया गया। इस 'पवित्र' दिन पर, शासकों को अन्य शासकों पर चढ़ाई करने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाता था, जिसे 'दैवीय रूप से निर्धारित कार्य' माना जाता था। (या सरल शब्दों में, निचले स्तर के सैनिकों को लूट और तबाही के माध्यम से अपनी जीविका कमाने का अवसर प्रदान करना)।
इन आवधिक आक्रमणों की अमानवीय क्रूरता, साथ ही युद्ध के समय किसी भी प्रकार के नागरिक नैतिकता की पूर्ण अनुपस्थिति, संघर्षरत गरीबों की दयनीय स्थिति को और अधिक खराब कर देती थी। निष्ठुर उपहास और हिंसक लालच (अक्सर जीविका की अत्यधिक आवश्यकता) ने आम जनमानस को एक ही सूर्य के नीचे जीवित रहने के लिए संघर्ष करने पर विवश कर दिया। ऐसे संगठित और अमानवीय युद्धों के सामने लोग पूरी तरह असहाय हो जाते थे।
लेकिन एक अंतर था।
नए आक्रमणकारियों की प्रवृत्ति महिलाओं के व्यापक शोषण की थी। विशेष रूप से, उन्होंने स्थानीय धार्मिक आस्थाओं को पूर्णतः तिरस्कृत किया और धर्मांतरण को जबरन थोपने में अधिक रुचि दिखाई। इस प्रकार की विशेषताएँ, जो भारत में पहले कभी नहीं देखी गई थीं, नए युद्धों को एक नए आयाम में ले गईं।
प्राचीन हिंदू शासकों के संगठित युद्धों में, उनकी संपत्ति, पहचान, घर, समाज, सम्मान, पारिवारिक प्रतिष्ठा और पूर्वजों की मान्यताएँ उनके साथ रहती थीं। वे समय के साथ अपने दुखों को सहन कर लेते थे क्योंकि वे पराजित भले ही होते थे, लेकिन उनका पूर्णतः अपमान नहीं होता था और वे अपने देवताओं तथा समाज से बहिष्कृत नहीं किए जाते थे। अपमान व्यक्तिगत या किसी कुल विशेष तक सीमित रहता था, लेकिन आम जनता पर इसका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता था।
फारसियों, पार्थियों, यूनानियों, कुषाणों और बैक्ट्रियनों ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ बस गए। वे एक प्रबुद्ध जनता और समृद्ध भूमि में आत्मसात हो गए।
लेकिन उत्तर-पश्चिम से आने वाले नए शत्रुओं ने पहले अज्ञात विध्वंसक तरीके अपनाए।
इस भीषण और संपूर्ण आक्रमण के सामने, अब अपने-अपने शासकों की सुरक्षा से वंचित गरीब लोग पूरी तरह असहाय हो गए। उनके धर्म को बलपूर्वक छीना गया। उन्होंने कई तरह की यातनाएँ सही, लेकिन उनके पूर्वजों के धर्म का जबरन नाश किया जाना उनके लिए सबसे बड़ा अपमान था। इसके परिणामस्वरूप एक गहरी सामाजिक दरार पैदा हुई।
जब इस अपमान के साथ-साथ उनके ही लोगों ने उन्हें उनके पुराने सामाजिक स्थान से वंचित कर दिया और बिना किसी गलती के समाज से बहिष्कृत कर दिया, तो उन्होंने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया। यह छिपा हुआ क्रोध उनके व्यक्तित्व में गहराई तक बैठ गया और कुंठा में बदल गया। इसी हताशा में उन्होंने सोचा कि इस छलपूर्ण और हृदयहीन सामाजिक ढांचे को नष्ट कर देना ही उचित होगा।
इसके अलावा, उन्हें एक और अधिक तीव्र अपमान सहना पड़ा। यह अपमान तिरस्कार और घृणा से भरा हुआ था। उनके पूर्व साथी, भाई, और रिश्तेदार—जो अधिक भाग्यशाली थे और जिन्होंने किसी प्रकार अपनी पहचान, सम्मान और धर्म को बचा लिया था—अब अत्यंत क्रूर और निर्दयी बन गए। वे स्वयं को 'देवताओं के प्रिय' समझने लगे और अपने आपको अधिक शुद्ध, अधिक श्रेष्ठ और अधिक चतुर मानने लगे। पीड़ित और परिवर्तित व्यक्ति उन्हें बाहरी शत्रु से भी अधिक पराया और घृणास्पद लगने लगे।
इस तरह, हिंदू समाज दो अलग-अलग सामाजिक संरचनाओं में विभाजित हो गया।
प्राचीन हिंदू समाज की एकता टूट गई और यह एक जटिलता में फंस गया, जिससे आज तक हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। सामाजिक सुधारकों के लिए यह हमेशा से एक स्वप्न रहा है कि हिंदू और हिंदू धर्म से परिवर्तित लोग एक साथ रहें, लेकिन यह सामाजिक संकट इतना गहरा है कि संतों, राजनीतिज्ञों और सुधारकों की सदियों की कोशिशें विफल रही हैं।
अंततः, जिन लोगों को समाज ने बहिष्कृत किया था, उन्होंने अपनी संगठित शक्ति से स्वयं को सुदृढ़ किया और कई बार शासकों के प्रिय समूहों में स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार, हिंदू भारत सामाजिक रूप से विभाजित हो गया और यह विभाजन स्थायी बन गया।
IX
इस प्रकार की बड़ी सामाजिक उथल-पुथल से पहले हिंदू समाज जीर्ण-शीर्ण, निरुत्साहित, भ्रमित और हतप्रभ था। जब पहले से संकटग्रस्त समाज पर विदेशी आक्रमणों की नई लहरें पीछे से टूट पड़ीं, तो धर्मांतरित असंतुष्टों के नए सामाजिक समूह ने इसे हर प्रकार से चुनौती दी।
इस क्रूर आक्रमण की नई तकनीक के समक्ष—जहाँ लूट और विध्वंस ही मूल उद्देश्य थे—जब इसे एक और प्रलोभन मिला, अर्थात् ‘एकमात्र सच्चे धर्म’ में परिवर्तित होने की जबरन कोशिश, तो यह तथाकथित सशक्त हिंदू सामाजिक संरचना को पूरी तरह हिला देने वाला था। यह समाज पूरी तरह भ्रमित होकर बिखर गया और शर्मनाक अव्यवस्था में घुलकर विलुप्त हो गया।
इस प्रकार के निर्मम उन्माद का प्रतिरोध करना व्यर्थ था, क्योंकि यह लूट और खजाने की असीम भूख से प्रेरित था। महिलाओं के अपहरण और उत्पीड़न ने इस भयावह तकनीक को और अधिक वीभत्स बना दिया।
परंतु हार में भी हिंदू वीरता ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने में संकोच नहीं किया। उन्होंने अपनी संपत्ति, महिलाओं और बच्चों तक को बचाने के प्रयास में अकल्पनीय कीमत चुकाई—कई बार स्वयं अपने ही हाथों से उनका अंत कर दिया।
प्रतिरोध व्यर्थ था; बलिदान महान था। लेकिन यह बुद्धिमानी नहीं थी। इस रणनीति ने निश्चित रूप से उन्हें युद्ध के गौरव से वंचित कर दिया, लेकिन यह आंशिक रूप से उनके पुरुषवादी अभिमान और सम्मान की रक्षा का एक प्रयास था।
लेकिन इतना त्याग करने के बावजूद वे सामाजिक ठहराव से बाहर नहीं आ सके, न ही वे एक नए बंधुत्व से बंधे एक मजबूत समाज के रूप में संगठित हो सके। वे ऐसा कर सकते थे, यदि वे चाहते, और इस प्रकार आगे के हस्तक्षेपों को रोक सकते थे।
उन्होंने यह पहले भी किया था—यूनानी और शक आक्रमणों के समय; फिर कुषाण और हूणों के समय। वे जानते थे कि सामाजिक अव्यवस्था को आत्मसात कर पुनर्संगठित कैसे किया जाता है। देवलस्मृति ने इसका मार्ग सुझाया था।
यह समझ से परे है कि किस प्रकार यह नकारात्मक मानसिकता आत्मसात करने की स्वस्थ प्रवृत्ति से अधिक संरक्षणवाद को प्राथमिकता देने लगी, और संकीर्ण स्वार्थ को सामूहिक कल्याण से ऊपर रख दिया।
एक सामाजिक जड़ता ने महान भारतवर्ष को जकड़ लिया था। इससे पहले कि अंग्रेज समुद्री मार्ग से नए आक्रमण लेकर आते, भारत का सामाजिक ताना-बाना पहले ही दो भागों में विभाजित हो चुका था। और यह विभाजन तब से स्थायी बना हुआ है, हालाँकि यह आश्चर्यजनक है कि समाज की आत्मा अब भी जीवित है। आध्यात्मिक रूप से, भारत अब भी एक है।
जो लोग पूर्ण विनाश और पूर्ण अपमान के बीच फँस गए थे, उन्होंने विजेताओं के धर्म को स्वीकार कर लिया। जो किसी तरह अपनी पहचान बचाने में सफल हुए और जिन्होंने जबरन धर्मांतरण से बचने की कोशिश की, वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पीड़ित हुए। भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से हिंदू गौरव, फिर कभी सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की शांति नहीं जान सका। (क्या यह राजनीतिक स्थिरता वास्तव में पहले कभी रही थी?)
इस विनाशकारी संघर्ष में सबसे अधिक पीड़ित श्रमिक वर्ग था—चाहे वे धर्मांतरित हों या न हों। यह वर्ग—मजदूर, मछुआरे, नाविक, कारीगर, बुनकर, गायक, संगीतकार, राजमिस्त्री, चर्मकार, मोची, पानी ढोने वाले, घरेलू सेवक, रसोइये, दास, और अंततः वे महिलाएँ जिन्हें हृदयहीन धार्मिक संस्थाओं ने छोड़ दिया था—सभी इस त्रासदी में सबसे ज्यादा पिसे।
ये अभागी महिलाएँ, जो अपनी कला, प्रतिभा और आकर्षण में निपुण थीं (अधिकतर उच्च और मध्य वर्ग की पृष्ठभूमि से), सेक्स-पिपासु विदेशी सैनिकों के सामने असहाय हो गईं और जबरन धर्मांतरित कर दी गईं। वे पारंपरिक हिंदू समाज से अलग कर दी गईं और बिना आश्रय के पक्षियों की भाँति हर गुजरती हवा का शिकार बनने लगीं।
परंतु उनकी कलात्मक क्षमताएँ और शारीरिक आकर्षण उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने रक्तपात और बलात्कार से अस्थायी राहत पाई और धीरे-धीरे एक स्थायी ग्राहक वर्ग विकसित किया। लेकिन समाज ने उन्हें जबरन हाशिए पर डाल दिया, और वे एक अलग समुदाय के रूप में उभर आईं।
जिनका जीवन कभी भव्य मंदिर परिसरों का हिस्सा था, वे मंदिरों के विध्वंस के बाद अपना आवास इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थीं। उन्होंने बिखरने से इनकार कर दिया और एक समुदाय के रूप में संगठित रहीं। इसी तरह उन्होंने मंदिर परिसर के निकट अपनी जगह बनाए रखी, जिसे अब दलमंडी कहा जाता है।
आज दलमंडी दाल (अनाज) नहीं बेचती। यहाँ की बस्तियाँ पुराने बाजार क्षेत्र तक फैल गईं, जो अब विदेशी वस्त्रों और लक्जरी उत्पादों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है।
इस दुखद घटनाक्रम का परिणाम यह हुआ कि एक क्षेत्र, जो कभी धार्मिक सेवा के लिए समर्पित युवतियों का निवास था, वह धीरे-धीरे ‘वेश्यावृत्ति’ के केंद्र में बदल गया। वे कन्याएँ, जिन्हें उनके धर्मपरायण माता-पिता देवताओं की सेवा के लिए अर्पित करते थे, एक बाजार का हिस्सा बन गईं।
ये अभागी स्त्रियाँ, जिनमें से अधिकांश प्रतिष्ठित और संपन्न परिवारों से थीं, कालांतर में वृद्ध और रोगग्रस्त हो गईं। जब वे ‘अप्रयोज्य’ हो गईं, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उनके पास जाने को कोई स्थान नहीं था, और अंततः उन्हें भी जबरन धर्मांतरित कर दिया गया।
कुछ ने अपने नए धर्म और जीवन को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि इससे उन्हें संरक्षण और सुरक्षा मिली। शायद वे भीतर ही भीतर यह सोचकर सांतवना पाती थीं कि यदि देवता उनकी रक्षा नहीं कर सके, तो शायद मनुष्य कर सकते हैं।
इस महाकाय त्रासदी की वास्तविकता और गंभीरता ने वाराणसी के सामाजिक ताने-बाने पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। धीरे-धीरे, मंदिर परिसर के आसपास ‘महिलाओं का एक गाँव’ बस गया, जहाँ से एक नया बाजार विकसित हुआ—एक ऐसा बाजार, जिसने सदियों से जीविका चलाई।
यहीं से एक प्रतिष्ठित कला-संस्कृति की समृद्ध परंपरा विकसित हुई। वाराणसी की गणिकाएँ न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपने संगीत, नृत्य और कला के लिए भी प्रसिद्ध हो गईं।
और यही कारण है कि आज भी, प्राचीन विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास वाराणसी का ‘रेड लाइट एरिया’ खड़ा है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में आज भी बढ़िया संगीत, इत्र, रेशम, आभूषण, फर्नीचर, चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित व्यवसाय फल-फूल रहे हैं।
इसका अस्तित्व इस बात की याद दिलाता है कि कैसे एक समर्पित धार्मिक समाज की स्त्रियाँ समय की क्रूरता का शिकार बनीं। हम सबने धीरे-धीरे और निष्ठुरता से उनके अस्तित्व को हाशिए पर डाल दिया, और वे समाज के राक्षसों की भेंट चढ़ गईं।
लेकिन मंदिर तो ढह गया, पर दलमंडी नहीं।
यह वाराणसी का एक दुखद स्मारक है—उन गौरवशाली दिनों की याद दिलाने वाला जब इस मंदिर में समाज के सबसे पवित्र प्रसाद के रूप में हिंदू कन्याएँ अर्पित की जाती थीं।
इस विषय पर गहराई से विचार करने के लिए, हमें इसे एक व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।
9.रुद्रवास
I
काशी-कोसल का युद्ध लगभग पाँच सौ वर्षों तक (लगभग 655-1155 ईस्वी) चलता रहा होगा। हमें ज्ञात है कि कुषाण, गुप्त, पुष्यभूति (थानेसर) और प्रतिहार वंश (106-1018 ईस्वी) के शासनकाल में काशी और सारनाथ को अनेक राजकीय अनुदान प्राप्त हुए थे।
इन 'अनुदानों' का वाराणसी से संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वाराणसी की भूमि को 'दान' नहीं किया जा सकता था, और न ही इसे स्वीकार किया जा सकता था। वाराणसी स्वयं शिव (शिव-गणों) की थी और इसे केवल 'शिवों' या 'शिवगणों' के लिए एक विशिष्ट स्थान माना जाता था। अतः वाराणसी में भूमि अधिग्रहण करना अत्यधिक जोखिमपूर्ण कार्य था।
यद्यपि पाल और सेना वंश के शासक शैव परंपरा से जुड़े थे, फिर भी उन्होंने सारनाथ के जैन और बौद्ध मंदिरों को भारी दान दिया। किंतु यह उल्लेखनीय है कि पालों और सेनाओं द्वारा किसी हिंदू मंदिर को ऐसा कोई बड़ा अनुदान देने का प्रमाण नहीं मिलता।
हालाँकि, उस काल में कई मठ, स्तूप और मंदिरों का निर्माण हुआ था और इन्हें अलंकरण भी प्रदान किया गया था, लेकिन वाराणसी की पहाड़ियों में किसी जैन या बौद्ध अनुदान का कोई प्रमाण नहीं मिलता। रुद्रवास वह क्षेत्र था जिसे उन्होंने भी अछूता छोड़ दिया था। संभवतः इसका कारण वाराणसी की प्राचीन कापालिक-भैरव परंपराएँ थीं। बंगाल के शैवों के लिए अति-वीर-अघोर-तंत्र उपयुक्त नहीं थे। यहाँ तक कि आज भी, दलमंडी के व्यस्त बाजार के मध्य में एक 'अघोरी टकिया' स्थित है।
वाराणसी ने सामान्यतः स्थापत्य या मूर्तिकला संबंधी अलंकरणों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। भैरव-अघोर परंपराओं के अनुसार, यहाँ किसी देवता की मूर्ति या मंदिर की प्राचीन परंपरा नहीं थी। केवल शिवलिंग को ही प्रतिष्ठित किया जाता था। औपचारिक देवताओं और मंदिरों का निर्माण संभवतः शक-युग के बाद प्रारंभ हुआ, विशेष रूप से प्रतिहार, पाल, सेना और गहड़वाल राजवंशों के लगभग 1200 वर्षों के दौरान। किंतु ये गतिविधियाँ मुख्यतः मच्छोदरी और मंदाकिनी क्षेत्र तक ही सीमित रहीं।
हालाँकि, हड़प्पा संस्कृति में हमें देवताओं के जूमॉर्फिक (पशु-आकृतियाँ) और एंथ्रोपोमॉर्फिक (मानव-आकृतियाँ) स्वरूपों के प्रमाण मिलते हैं, किंतु प्राचीन हिंदू धर्म में अभी तक ऐसी मूर्तियों की विशेष प्रवृत्ति विकसित नहीं हुई थी।
वाराणसी भारतीय इतिहास में हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी बस्ती रही है और इसके स्थानीय निवासी निश्चित रूप से ब्राह्मणीय आर्य परंपरा से भी पहले के थे। इसलिए उन कालों में वाराणसी में मूर्ति-पूजा की उपस्थिति अधिकतर एक काल्पनिक अवधारणा ही हो सकती है।
II
शास्त्रों और अन्य अभिलेखों के अनुसार, वाराणसी को योगियों और विद्वानों के लिए एक वन्य आश्रय स्थल के रूप में देखा जाता था। वे गुफाओं और वनों में ध्यान और आध्यात्मिक साधना करते थे।
ये प्राचीन निवासी (संभवतः हड़प्पा परंपरा से जुड़े), नाग, गण, जिन्हें महेश्वर-कापालिक भी कहा जाता था, प्रकृति के समीप रहना पसंद करते थे। उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन विकसित किया जिसमें प्रकृति, अप्सराएँ और तांत्रिक रहस्यवाद प्रमुख भूमिका निभाते थे।
यह संपूर्ण वातावरण यह विश्वास दिलाता है कि यह स्थान तंत्र-साधना, मिथकों और रहस्यवाद के प्रचार-प्रसार के लिए आदर्श था। इस संदर्भ में, वाराणसी एक तंत्र-केन्द्र के रूप में उभरती है, जहाँ तंत्र को तीन पारंपरिक धाराओं—सावचारा, वीरचारा और शिवचारा—के अनुसार साधना की जाती थी। ये धाराएँ क्रमशः तामसिक, राजसिक और सात्त्विक प्रवृत्तियों का पालन करती थीं।
यहाँ के मूल निवासियों का ध्यान जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने पर केंद्रित था। मृत्यु का अज्ञात भय उन्हें ईश्वर और प्रार्थना की ओर प्रेरित करता था। भोजन, वर्षा, फसल—इनकी हानि उन्हें प्रार्थना करने के लिए बाध्य करती थी। ये पहाड़ी निवासी जानते थे कि शिव का डमरू दोनों दिशाओं में बजता है—सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु।
तंत्र अत्यंत व्यावहारिक, ग्रामीण और आदिम था। यह पूर्व-आर्य संस्कृति का हिस्सा था। उन प्राचीन समुदायों को गण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, गुह्यक, कपाल, शिव और अघोर के रूप में जाना जाता था, और वाराणसी इनका प्रमुख केन्द्र था।
इन्हें जिन देवताओं की आराधना करनी होती थी, वे भी मूलभूत प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े थे—पृथ्वी, जल, वर्षा, नदियाँ, वृक्ष, गुफाएँ, झरने, प्रेम, सेक्स और मानव शरीर। वे यह मानते थे कि कामना और प्रेम की शक्ति को पहचानना और नियंत्रित करना आवश्यक है, अन्यथा यह विनाशकारी बन सकती है।
तिब्बती बौद्ध धर्म में यमांतक की भयानक छवि और भगवद गीता के ग्यारहवें अध्याय में 'काल' के रूप में वर्णित महाकाल इसी शक्ति की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं।
स्त्री को उन्होंने प्रेमिका, माता, सखा और एक बहुआयामी सृजनशील शक्ति के रूप में देखा। परंतु स्त्री को उन्होंने विनाशकारी शक्ति के रूप में भी स्वीकार किया। यह शक्ति मानव शरीर के भीतर भी कार्य करती थी और इसे पहचानना और उपयोग करना आवश्यक था।
इसलिए उन्होंने इस शक्ति की साधना को 'यहाँ और अभी' प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस की। तांत्रिक परंपरा सदा शरीर पर केंद्रित रही है। तांत्रिक साधकों के लिए पृथ्वी और आकाश पोषक थे, और शरीर एक अज्ञात आत्मा का मंदिर।
तंत्र के लिए महत्वपूर्ण था—जल को जल की तरह देखना, जीवन को जीवन की तरह, मृत्यु को मृत्यु की तरह, पुरुष को पुरुष की तरह और स्त्री को स्त्री की तरह।
काशी—एक 'प्रकाश-स्थली'
काशी नाम का अर्थ भी
'प्रकाश' से जुड़ा हुआ है।
यह वह स्थान था जहाँ
ज्ञान और चेतना का रहस्य
उद्घाटित हुआ। इसलिए काशी को
एक देवी का रूप दिया
गया।
यहाँ, भावनाएँ रुक जाती हैं। आत्म-अहंकार व्यक्ति से परे चला जाता है। दुनिया का अनुभव एक नए यथार्थ में बदल जाता है।
इस प्रकार, वाराणसी केवल एक शहर नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु, प्रेम और तंत्र, आत्मा और शरीर के गूढ़ रहस्यों का केन्द्र रहा है।
रुद्रवास केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा थी, जो तंत्र-साधना, रहस्यवाद और प्रकृति की आराधना से गहराई से जुड़ी हुई थी। यह स्थान न केवल प्राचीनतम समुदायों का आश्रय था, बल्कि यह भारत में तंत्र परंपरा के जीवंत केंद्रों में से एक था।
III
वाराणसी के पूर्व-आर्य मूल निवासी प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने की कला में निपुण थे। वे जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते थे जैसा कि प्रकृति चाहती है—बिना किसी बाहरी आडंबर के। वे भोग-विलास से परिपूर्ण थे, लेकिन वासना से मुक्त थे। (यह एक अत्यंत कठिन साधना थी।)
उन्होंने कृत्रिम सामाजिक बंधनों, छल, धार्मिक पाखंड और तथाकथित सामाजिक परिष्करण को सिरे से नकार दिया। आज भी, उत्तर कोसल (अर्थात् अयोध्या-मथुरा और विशेष रूप से वाराणसी) के लोगों में इन विशेषताओं के कुछ चिह्न देखे जा सकते हैं। वे अपनी खुली सोच, जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण और स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे स्वतंत्रता का अनुभव करते थे, स्वतंत्र रूप से जीते थे, स्वतंत्र रूप से सोचते थे और एक अनासक्त शुद्ध चेतना तक पहुँचने में सक्षम थे।
उनके दृष्टिकोण में द्वैत के पंख अनादि सत्य के विशाल आकाश को छूते थे। वे अनुशासन और स्वच्छंदता, नियम और स्वतंत्रता, तथा उपासना और प्रबल जीवन-शैली को एक साथ मिलाने में सक्षम थे।
उन्होंने प्रकृति को सीधे और निःसंकोच देखने को प्राथमिकता दी। उनके लिए सत्य नग्नता में खड़ा होना चाहिए था—बिना किसी आडंबर के। सत्य, उनके अनुसार, स्वाभाविक भव्यता में मुक्त होना चाहिए—कठोर दंड देने वाला, लेकिन अंततः दयालु और कृपालु।
ये वन, पर्वत और नदियों के उपासक थे, जिन्होंने अपने शरीर की लयबद्ध उत्तेजना को भक्ति में परिवर्तित कर दिया था। उनके लिए, शरीर का आनंद सृष्टि के दिव्य मिशन के आनंद की अभिव्यक्ति था।
शरीर के माध्यम से परम आनंद तक पहुँचना, लेकिन शरीर से बंधे बिना रहना—यही उनके लिए आध्यात्मिक उपलब्धि का शिखर था।
वे सदाशिव, शंभु थे—माँ की गोद में खेलते हुए शिशु। इसलिए उनके लिए वृक्ष, उपवन, गुफाएँ, नदियाँ और झीलें अत्यधिक महत्व रखती थीं। इन्हीं माध्यमों से वे परम सत्य तक पहुँचते थे।
वे किसी भी प्रकार के पुरोहितवादी यज्ञों में विश्वास नहीं रखते थे, न ही वे ईंट-पत्थर, सोने-चाँदी के ऊँचे टॉवर बनाकर अपने हाथों से गढ़े गए देवताओं और देवियों को उनमें कैद करना चाहते थे।
मंदिर, चैत्य, मूर्तियाँ और शास्त्रों के जटिल शब्द उनके लिए नहीं थे। वे एक मौलिक और प्राचीन जीवन जीने वाले लोग थे, जो अपने अनगढ़ रूप में देवताओं की आराधना करते थे—और आश्चर्यजनक रूप से, उनका ईश्वर उनके लिए कार्य भी करता था।
IV
वाराणसी का वन्य क्षेत्र, आनंदकाननम, उन साधकों के लिए एक विशेष स्थान था जो आनंद और पीड़ा, जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहते थे। यह स्थान अपने निवासियों को माँ की गोद-सी सुरक्षा और एक स्त्री के संग-साथ का स्नेह प्रदान करता था।
उन्होंने इस विचार के अनुसार जीवन जिया और उपासना की—"हर चीज़, हर व्यक्ति अपने स्थान पर और अपनी वास्तविक महत्ता के अनुसार"।
उनकी मुक्ति
प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनगिनत खिड़कियों को खोलकर प्राप्त हुई।
उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर
के बंधनों से मुक्त कर
दिया और प्रकृति की स्वतंत्र वायु में प्रवाहित किया,
जिससे उनकी बदली हुई दृष्टि
में संसार अत्यंत छोटा, नगण्य और लगभग अस्तित्वहीन लगने लगा—एक अपार, अथाह और अकल्पनीय ब्रह्मांड के समक्ष।
("रहस्यम् ह्येतदुत्तमम्"—"यह एक महान रहस्य है"—भगवद्गीता)।
उन्होंने एक सरल, निर्भीक मार्ग चुना—शिव का मार्ग। यह मार्ग सीधे माँ की सुरक्षा और आश्रय तक ले जाता था। यह उनका धर्म, उनकी आस्था और उनकी साधना थी—यह भय और आसक्ति से परे, एक अंतरतम से मुक्त, आनंद और मुक्ति तक पहुँचने का मार्ग था।
ऐसे समाज में मंदिर, चैत्य, मूर्तियाँ, पंडितों का झुंड, या किसी भी प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं थी।
शिवों के इस विशेष मार्ग में देवता को प्रसन्न रखने के लिए युवतियों का दान या विशेष अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं थी। स्त्री उनके लिए केवल भोग और वासना का माध्यम नहीं थी, बल्कि एक पूर्णतः पवित्र सहभागी थी। उनके विचार में यदि देवताओं में भी वासना होती, तो वह भी मात्र वासना ही होती।
प्राचीन काल में रुद्रवास में कोई भी मूर्ति-स्थापित देवता, कोई मंदिर, या कोई पवित्र तीर्थ (जहाँ पापी अपने पाप धो सके) नहीं था।
केवल तब, जब स्कंद, अगस्त्य जैसे ब्राह्मण, और दुर्वासा जैसे ऋषियों (जिनका उल्लेख काशी खंड में मिलता है) ने इन पवित्र स्थलों के महत्व को स्थापित करना प्रारंभ किया, तब जाकर रुद्रवास की आंतरिक महानता और गरिमा घमंडी आर्यों के लिए खुल सकी।
क्योंकि आर्यों के लिए, तब तक यह रहस्यमयी वन केवल भूतों और प्रेतों का निवास-स्थान था।
V
यह गैर-आर्य समुदाय वरुणा और उसकी घाटियों से दूर रहता था। वे रुद्रवास, आनंदकाननम्, अर्थात् गंगा के किनारे फैली पहाड़ियों पर टिके रहे।
जब नई सभ्यता के लोग अपनी 'श्रेष्ठ' संस्कृति के साथ आए, तो उन्होंने वरुणा के उत्तर से अपना विस्तार शुरू किया और केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्र तक पहुँचे, जहाँ उन्होंने शिखर पर अपने मंदिरों की स्थापना की।
जब ह्वेनसांग ने यात्रा की, तो उसने बौद्ध मंदिरों को पास ही स्थित पाया। जैन समुदाय ने अपने मंदिर वरुणा और गंगा के संगम पर बनाए थे।
रुद्रवास का मूल क्षेत्र और इसका पश्चिमी परिवेश ‘सभ्य लोगों’ के लिए निषिद्ध रखा गया था। तब से एक स्पष्ट सीमा-रेखा बनी रही, जिसका आज तक सम्मान किया जाता है। अठारहवीं सदी के अंत तक, केंद्रीय पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित वन्य दलदली क्षेत्र को 'सभ्य समाज' के लोग सावधानीपूर्वक टालते रहे।
इस क्षेत्र का विकास अठारहवीं सदी के मध्य में ही शुरू हुआ। (यहाँ तक कि वर्तमान सदी की शुरुआत में भी यह क्षेत्र वाराणसी का सबसे जंगली भाग माना जाता था। विश्वविद्यालय और बंगाली टोला क्षेत्र के निर्माण ने पहली बार यहाँ स्थिति को बदलने में योगदान दिया।)
पश्चिमी दलदली विस्तारों के साथ स्थित मैदानों में स्थिति अलग थी। वहाँ कई विशाल जल-स्रोत थे, जिन्हें रेवतीतड़ाग (रेउरीतालाब)पोखरा, तड़ाग, तालाब, कुंड आदि कहा जाता था। इनमें से प्रमुख थे—
● लक्ष्मीकुंड
● पितृकुंड
● वाल्मीकि कुंड
● मिश्रपोखरा
● पिशाचमोचन कुंड
● मातृकुंड
● लहरिया तालाब आदि।
जो लोग यहाँ रहते थे और इन जलस्रोतों को पवित्र मानते थे, वे स्थानीय नागवंशी और भैरव-शिव संप्रदायों से संबंधित थे।
आर्य संस्कृति के जटिल धार्मिक अनुष्ठान इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाए थे। यहाँ के गैर-आर्य समुदायों ने 'एनिमिज्म' (प्राकृतिक शक्तियों की पूजा) और तंत्र-साधना की अपनी परंपरा बनाए रखी थी और वे रहस्यमय अनुष्ठानों, तंत्र-मंत्र और जादू-टोने का अभ्यास करते थे।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से आए उपनिवेशवादी, जो वरुणा को पार करके वाराणसी पहुँचे थे, उनके लिए ये पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाटियाँ 'आतंककारी आत्माओं' से भरी थीं।
वाराणसी का एकमात्र मंदिर, जहाँ आज भी रक्त बलि की परंपरा जारी है, इसी क्षेत्र में स्थित है।
यही वह वन था, जहाँ संत गोस्वामी तुलसीदास ने ब्राह्मणों के हमलों से बचने के लिए शरण ली थी और यहाँ ही उन्होंने 'रामचरितमानस' की रचना पूरी की थी।
इस तरह की ऐतिहासिक घटनाएँ हमारे इस तर्क को बल देती हैं कि ये पहाड़ियाँ एक विशेष संप्रदाय के अनुयायियों का आश्रय थीं, जिसे 'पशुपति संप्रदाय' कहा जाता था।
इस संप्रदाय का संबंध हड़प्पा संस्कृति से था। इस संदर्भ में सर जॉन मार्शल, ऑरेल स्टीन, आर. डी. बनर्जी, हेनरिक ज़िमर, डी. डी. कोसंबी और ए. एल. बाशम के शोध उल्लेखनीय हैं।
लेकिन इस विभाजन ने ही आक्रमण को जन्म दिया। आर्य सभ्यता का सैन्य प्रसार शीघ्र ही इन पहाड़ियों तक पहुँचा। इस संघर्ष से उत्पन्न रक्तरंजित युद्धों का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है—
1. 'काशी खंड' (K. Kh.)
2. 'अग्नि पुराण' (Agni P.)
3. 'वायु पुराण' (Vayu P.)
4. 'मार्कंडेय पुराण' (Markandeya P.)
5. यहाँ तक कि 'महाभारत' (Mbh.) में भी।
इन युद्धों के कुछ प्रमुख उदाहरण—
● आर्य प्रमुख दक्ष द्वारा शिव पशुपति के विरुद्ध युद्ध।
● देवताओं द्वारा शिव से सहायता माँगना, ताकि वे असुरों के घृणा से उत्पन्न विष से बच सकें।
● शिव के गणों द्वारा पहाड़ियों को शिव-शक्ति के एकांत मिलन स्थल के रूप में चिह्नित करना (काशी खंड, अध्याय 26)।
● शिव के गणों, भूतों, पिशाचों और प्रेतों की सेनाओं के विरुद्ध देवताओं की सैन्य टुकड़ियों की भिड़ंत।
आर्य विस्तारवाद ने अंततः आनंदकाननम् को भी अपनी चपेट में ले लिया। विस्तारवाद हमेशा से आर्य रक्त में अंतर्निहित रहा है। काशी-कोसल के उपनिवेशवादी सदियों से इन सुंदर पहाड़ियों को हड़पने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार, उन्होंने यह कर भी लिया।
VI
यह परंपरा इतनी प्राचीन थी कि पीढ़ियों तक पवित्र आत्माएँ इन पहाड़ियों को ध्यान और साधना के लिए एक शांत आश्रय के रूप में उपयोग करती रही थीं। इसी कारण हर जलाशय, नदी-तट, जलधारा का उद्गम, संगम, यहाँ तक कि सबसे साधारण गुफा, टीला, झाड़ी, उपवन, तालाब और झील भी किसी न किसी विद्वान, ऋषि या संत के साथ वर्षों की संगति के कारण एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था।
वाराणसी, रोम, मक्का, यरूशलेम, लंदन या साइप्रस से भी अधिक, प्राचीन और प्रभावी तीर्थ स्थलों से भरी हुई है। इन स्थलों में से अधिकांश शैव परंपरा और गणों के प्रभाव से जुड़े हैं।
यह मान्यता फैल गई थी कि रुद्रवास की सभी चट्टानें, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है, स्वयं शिव के समान पवित्र हैं। भक्तों का विश्वास था कि वाराणसी की रेत 'आध्यात्मिक चुंबकत्व' से भरपूर है।
वाराणसी—जिसकी धूल तक स्वर्ण-धूल थी; जिसकी कंकड़ तक दिव्य थे; यहाँ की जल की सबसे छोटी बूँद तक अमृत और मधु के समान थी। यहाँ तक कि वाराणसी के कूड़े-करकट के पास घूमने वाले कुत्ते और सूअर, या इसकी नदी में रहने वाले कछुए और मछलियाँ भी एक ऐसे जीवन को प्राप्त थे, जिसकी ईर्ष्या वे कर सकते थे जो अभी वहाँ जाने की लालसा रखते थे।
जो कोई भी मोक्ष की खोज में था, वह इस नदी के किनारे जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता था। यदि युवावस्था में नहीं, तो कम से कम जीवन के उत्तरार्ध में, जब संध्या की छाया और अधिक फैलकर दूर के आकाश को और भी दूर धकेल देती है, और जब घेरती हुई अंधकारमय छायाएँ लंबी और रहस्यमयी होती जाती हैं, तब वाराणसी के तट की लालसा किसी भी 'प्रस्थान करते' हिंदू के मन को बेचैन कर देती है।
उनके लिए वाराणसी अंतिम पर्वत-शिखर थी, जहाँ से अज्ञात परे की बुलाहट की ज्योति को पकड़ना संभव था। यह त्यक्त और दुखी आत्माओं के लिए शांति के स्वर्ण-द्वार को खोलती थी, जहाँ से पीड़ित आत्मा को कभी लौटाया नहीं जाता था।
VII
यह रूपक जीवन और मृत्यु के वैदिक दृष्टिकोण को मूल निवासी गणों के दृष्टिकोण से अलग करने का एक और महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत करता है। यह 'परलोक' की अवधारणा और विवादास्पद पुनर्जन्म सिद्धांत से संबंधित है।
यह विचार, जो हिंदुओं के लिए अत्यंत प्रिय है, वैदिकों को विशेष रूप से परेशान करता हुआ प्रतीत नहीं होता। अथर्ववेद मृतकों के निपटान की एक प्रक्रिया को स्वीकार करता है। यह निर्गत आत्मा की शांति और मोक्ष की खोज, साथ ही पितरों के साथ अंतिम सामंजस्य की बात करता है। आश्वलायन गृह्यसूत्र में, अग्नि को एक शक्तिशाली पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है, जो मुक्त आत्माओं को अपने सशक्त पंखों पर उठाकर अंततः उन्हें पितृलोक तक पहुँचाता है। अथर्ववेद पितरों को अमर कहता है (VI.41.3; VII.76.4; X.56.4)।
पितर, जो देवताओं के समान महान हैं, वेदों के अनुसार, प्रकाशमय दिन और अंधकारमय रात्रि का निर्माण करते हैं। वे उषा (सुबह की लाली) के आगमन के लिए भी उत्तरदायी हैं।
प्रेतों की अवधारणा, आत्माओं के महिमामंडन, और व्यक्तिगत आत्माओं की मुक्ति एवं शांति के लिए विशेष अनुष्ठानों का निष्पादन, वैदिक परंपरा का अंग नहीं प्रतीत होता। प्रेत-कृत्य (मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले संस्कार) को सदैव दुनिया भर के आदिवासी समाज की एक विशेष संस्कृति के रूप में देखा गया है।
संपूर्ण विश्व के आदिम समाजों की यह विशेषता रही है कि वे एक बाहरी लोक की अवधारणा को मानते थे। उनका विश्वास था कि उनके दिवंगत प्रियजन एक नए संसार में भी उन वस्तुओं और साधनों की आवश्यकता महसूस करेंगे, जो उनके लिए जीवनकाल में प्रिय और आवश्यक थे।
चाहे यह विचार सही हो या गलत, सभ्यता को इसके कारण प्राचीन जीवन की अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। प्राचीन कब्रगाहों और समाधियों से अनेक भूली-बिसरी संस्कृतियाँ पुनर्जीवित हुईं।
लेकिन यह विचार ऋग्वैदिक लोगों पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सका। यदि अथर्ववेद में यह विचार मिलता भी है, तो हमें यह भी ज्ञात है कि अथर्ववेद को अन्य तीन वेदों (त्रयी) में बहुत बाद में जोड़ा गया था। पूर्वज-पूजा को हिंदू प्रार्थना-पद्धति में बहुत बाद में शामिल किया गया।
लेकिन आदिवासियों के लिए यह जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य और अनिवार्यता थी।
भागवत गीता, जो बहुत बाद की रचना मानी जाती है, उसमें आत्मा के आगमन और गमन का उल्लेख मिलता है (VIII.15-16, 19, 26; IX.3, 21)। यह स्पष्ट रूप से कहती है कि शरीरधारी आत्मा का अंतिम भाग्य उन विचारों से निर्धारित होता है, जो मृत्यु के अंतिम क्षणों में मन को विचलित कर रहे होते हैं (गीता VIII.5-6)।
पुनर्जन्म, मृतकों के लिए प्रार्थना, श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराना, तथा दान की अवधारणा—सभी इसी विचार से उत्पन्न हुए हैं।
मृत्योत्तर संस्कारों का पूर्ण समर्थन हमें विष्णु भागवत, वराह, गरुड़ और ब्रह्मवैवर्त पुराण (प्रथम से ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी तक) के काल में ही प्राप्त होता है। प्रेत (पितरों से भिन्न), पिंडदान आदि के उल्लेख महाकाव्यों में भी मिलते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इन्हें पुरोहितों के बाद के समय में जोड़े गए अंश मानते हैं।
वैसे भी, गण-भूतों की आदिवासी प्रेत-संस्कृति को आर्य परंपरा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया महाभारत के व्यास, रामायण के वाल्मीकि, या पुरुरवा-ययाति-मंधाता-नहुष-इक्ष्वाकु वंशों से भी पहले की है।
मृतकों को स्मरण करने और सम्मान देने की परंपरा, तथा यह चिंता कि मृत आत्माओं को सुविधा प्रदान की जाए, आदिम समाज व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक थी।
इसीलिए, वाराणसी की महत्ता एक 'सुरक्षा-घाटी' के रूप में और भी बढ़ जाती है। वाराणसी का महत्व इसके 'महाश्मशान' के रूप में प्रतिष्ठा से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह स्थान पुनर्जन्म के बंधनों से तत्काल मुक्त होने की निश्चित गारंटी के रूप में स्वीकृत है।
स्पष्ट रूप से, ये सभी अवधारणाएँ पूर्व-वैदिक सिद्धांत हैं। जब आर्य प्रवासियों ने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया, तो उन्होंने स्वयं को महाश्मशान परंपरा में सम्मिलित कर लिया। यह एक और प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वाराणसी का मूल निवास गैर-आर्य, मूलनिवासी समुदायों द्वारा किया गया था।
वाराणसी को सदैव एक पवित्र स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में, यह 'पवित्र स्थलों का भी पवित्रतम स्थान' है—वह अंतिम स्थान, जहाँ अंतिम साँस ली जा सकती है और अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान किया जा सकता है।
यहाँ मृत्यु स्वयं आत्मा को धन्य और पवित्र बना देती है। इसलिए, पीड़ित आत्मा को किसी विशेष ब्राह्मणीय अनुष्ठान या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। मूल निवासी यह नहीं चाहते थे कि वाराणसी में मृत्यु के नाम पर ब्राह्मणवादी शोषण हो।
इस 'परलोक जीवन' के प्रति अनूठे दृष्टिकोण ने वाराणसी की मानसिकता में एक विशिष्ट प्रभाव डाला है। यह रुद्रवास की पूर्व-वैदिक संस्कृति की पुष्टि करता है, जहाँ पूर्व-आर्य विश्वासों का गहरा प्रभाव था। यदि और अधिक प्रमाणों की आवश्यकता हो, तो वाराणसी की महिमा एक अंतिम मुक्ति-स्थल के रूप में, और विशेष अंतिम संस्कारों की परंपरा एक और प्रमाण प्रस्तुत करती है।
वाराणसी की धूल उन असंख्य संतों और साधुओं की अस्थियों को संजोए हुए है, जिन्होंने इसकी धुंधली गलियों से होकर यात्रा की और इसके पवित्र जल में स्नान किया। यहाँ की आत्मा में आध्यात्मिकता रची-बसी है।
हालाँकि पितरों की विस्तृत पूजा प्रणाली रुद्रवास के अतीत को दर्शाती है, किंतु जब हम देखते हैं कि यहाँ प्रेतों को, न कि पितरों को, अधिक सम्मान दिया जाता था, तो यह इसकी अत्यंत प्राचीन पूर्व-वैदिक संस्कृति को स्थापित करता है।
वाराणसी के जीवन में दोनों अवधारणाएँ—प्रेत (मध्यवर्ती आत्माएँ) और पितर (पूर्वज)—महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
● पितर (Manes) की पूजा ऋग्वैदिक संस्कृति से संबंधित है।
● प्रेतों (असहाय आत्माओं) की अवधारणा आदिम पूर्व-वैदिक समुदाय से आई है, जिनके लिए वाराणसी एक पूर्वजों का घर थी।
VIII
वाराणसी में किसी भी वैदिक देवता के नाम पर कोई संरचना नहीं बनाई गई, न ही कोई पवित्र तीर्थस्थल स्थापित किया गया। वरुण, अग्नि, यम, इंद्र, मातरिश्वा, अश्विनीकुमार, नासत्य या यहाँ तक कि सोम तक को किसी भी भौतिक स्मारक द्वारा सम्मानित नहीं किया गया। यदि संयोगवश किसी वैदिक देवता का अस्तित्व वाराणसी के मानचित्र पर दर्शित हुआ, तो उसे लिंग-रूप में परिवर्तित कर पूजा जाना पड़ा, जैसे—सोमेश्वर, शुक्रेश्वर, ध्रुवेश्वर आदि।
केवल रुद्र, रुद्र-गण, और निश्चित रूप से देवी (भूता-संगिनी रूप में) ही वे दिव्य इकाइयाँ थीं, जो वाराणसी के प्रारंभिक उपासकों के लिए मायने रखती थीं।
वाराणसी का एक प्रसिद्ध नाम "रुद्रवास" (रुद्र का निवास) है। महाश्मशान के साथ मिलकर यह नाम वाराणसी की पूर्व-वैदिक संस्कृति को लगभग पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। रुद्र की सह-अभिव्यक्ति भवानी, जिसे विशाला, ललिता, त्रिपुरेश्वरी, विशालाक्षी के नाम से भी जाना जाता था, वाराणसी की मुख्य देवी थी।
इन दो प्रधान देवताओं—रुद्र और शक्ति—के साथ उनके अनुचर और संरक्षक (गणेश, भैरव) भी प्रतिष्ठित थे, और ये सभी वाराणसी के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों का केंद्र बने।
किन्तु इनके लिए कभी भी कोई भव्य मंदिर आवश्यक नहीं था। वास्तव में, ये अधिकतर वृक्षों के नीचे, सड़क चौराहों पर, जलस्रोतों, झरनों, पहाड़ियों और टीलों के शिखरों पर स्थापित थे।
बाद में यह स्पष्ट होगा कि वाराणसी के अधिकांश प्राचीन तीर्थस्थल पूरी तरह से खुले और प्राकृतिक परिवेश में स्थित थे, जहाँ मानव की दुर्बलताएँ—अहंकार, सत्ता, वैभव या प्रदर्शन—कोई स्थान नहीं रखती थीं।
प्रारंभिक देवताओं की कोई स्पष्ट मूर्त-रूप आकृति थी? संभवतः नहीं, लगभग नहीं। इन प्राकृतिक स्थलों को किसी भी विशिष्ट मूर्तिकला, मानव-आकृति, या कलात्मक उत्कृष्टता से नहीं सजाया गया था। यदि कोई प्रतिष्ठित रूप था, तो वह था लिंग-शिला (आयताकार स्तंभ-रूप) और वीर-स्वरूप। इसके अलावा, नंदी के रूप में बैल या नाग के रूप में सर्प को ही जनसाधारण की श्रद्धा प्राप्त थी।
मानवीय रूपों में देव-प्रतिमाओं की पहली उपस्थिति शक-युग के बाद, गांधार कला की बोधिसत्व आकृतियों के रूप में देखी गई।
इन यूनानी-शक प्रभाव वाली कलाकृतियों का प्रभाव इतना गहन, प्रभावशाली और भावनात्मक था कि पहले से ही हड़प्पा अनुभवों से परिचित भारतीय समाज ने इसे तुरंत अपना लिया।
कुछ विदेशी विद्वानों ने शिव की पहचान डायोनिसस या हेराक्लीस से, विष्णु की बृहस्पति से, और सूर्य की अपोलो से जोड़ने में भी संकोच नहीं किया।
यूनानी और रोमन मुख्यतः पितृसत्तात्मक समाज थे। वे देवी या शक्ति को 'माँ' के रूप में पूजने में विशेष रुचि नहीं रखते थे। उनके लिए स्त्री देवियों का चरम स्वरूप वीनस, जूनो, एफ़्रोडाइट या मिनर्वा थीं, जो मातृ-भावना के बजाय विलासिता और भोग-वृत्ति की अधिक प्रतीक थीं।
प्राचीन रुद्रवास ने इन समस्त मूर्तियों और देव-प्रतिमाओं की जटिलताओं को दरकिनार कर दिया। रुद्रवास पूरी तरह से पूर्व-वैदिक, मौलिक और मूलभूत था। यह परंपरा लिंग-पट्टा (शक्ति-स्तंभ) के संयोग में अधिक सहज महसूस करती थी। पहाड़ी क्षेत्रों के रुद्र-शिव उपासक प्रकृति और उसके विभिन्न रूपों के समक्ष नतमस्तक होते थे।
वे 'आत्मवादी' (Animists) संप्रदाय के अनुयायी थे। एक शिला, कंकड़, गुफा, झरना या नदी उनके लिए पूजा और ध्यान के केंद्र थे। शिव की आदिम प्रतिमाएँ एक गोलाकार चबूतरे के केंद्र में स्थित शंक्वाकार प्रस्तर-चिह्न के रूप में थीं, जो सृष्टि और संहार के रहस्यों पर ध्यान केंद्रित करने का माध्यम थी।
यह मान्यता थी कि—
● "एक केंद्र" (शिव) होता है
● "एक वृत्त" (शक्ति) उसके चारों ओर सतत गति करता है
● "केंद्र स्थिर रहता है", जबकि वृत्त निरंतर परिक्रमा करता है
लिंग-पट्ट के प्रतीकवाद में—
● परमाणु के भीतर ऊर्जा का पहला स्पंदन, जो सृष्टि को विकसित करता है।
● एक ठोस शंक्वाकार पर्वत (लिंग) ऊर्जा क्षेत्र (पट्ट) के केंद्र में स्थित, जो सृजन और विनाश, अस्तित्व और शून्यता, पुरुष और प्रकृति के रहस्यमय संबंधों को दर्शाता है।
यह रूप "सभी कारणों के कारण" (Cause of all causes) की अवधारणा प्रस्तुत करता था—एक 'कोस्मिक टर्मिनल', जहाँ सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ मिलती हैं। यह प्रतीक जीवन की महानतम पहेली का उत्तर प्रस्तुत करता था।
आज भी, नियमित रूप से, ये प्रतीक वाराणसी और संपूर्ण भारत में अप्रत्याशित कोनों में उभरते रहते हैं, जहाँ भी ईश्वर का स्मरण किया जाता है। इन आध्यात्मिक स्थलों को अनेक महर्षियों की उपस्थिति का आशीर्वाद प्राप्त था।
अनेक नदियाँ और जलाशय, जो इन महापुरुषों की तपस्या से जुड़ी थीं, आज भी उनके स्मरण में जीवित हैं, जैसे— वशिष्ठ, गौतम, कपिल, कर्दम, दक्ष, दुर्वासा, अगस्त्य, व्यास, मार्कंडेय, दत्तात्रेय आदि।
वाराणसी के विशाल मंदिर और भव्य देवालय, जो आज देखे जाते हैं, संभवतः गुप्त, पाल, सेना और गहड़वाल शासकों के प्रयासों का परिणाम थे। यह बौद्धोत्तर शासकों द्वारा निर्मित संरचनाओं की नकल में निर्मित हुए। यह नवीन प्रवृत्ति वाराणसी के मौलिक शिव-उपासना रूप में एक नया आयाम जोड़ने का कार्य कर रही थी। वाराणसी, महाश्मशान, रुद्रवास, गौरीपीठ, आनंदकाननम, अविमुक्त इन सभी नामों के माध्यम से नए युग में प्रवेश कर रही थी।
रुद्रवास ने आनंदकाननम् के लिए मार्ग बनाया, और आनंदकाननम् ने अंततः वाराणसी के रूप में अपनी स्थिति सुनिश्चित कर ली।
IX
उत्तर भारत में सदियों से साम्राज्यों का उत्थान और पतन होता रहा। यहाँ अनेक युद्ध हुए, निपटे, और फिर छिड़े—वाराणसी भी इसका अपवाद नहीं थी। लेकिन वाराणसी के तपोवन को प्रायः इन संघर्षों से अलग रखा गया। इसका कारण रुद्रवास की पहाड़ियों में रहने वाले गुप्त, रहस्यमय और उग्र स्वभाव के लोगों से संबंधित कथाएँ थीं, जिन्हें भयानक अनुष्ठानों और विकट आचरण के लिए जाना जाता था।
इन लोगों की अज्ञात और अप्रत्याशित प्रवृत्तियों के कारण कोई भी जबरन उनके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं करता था। इस कारण विस्तारवाद केवल वरुणा नदी के तटों तक ही सीमित रहा। कोई भी इन वनों से घिरी पहाड़ियों में भीतर जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था।
इसलिए किसी को भी वाराणसी को "घर" बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया, सिवाय उन "अनंत यात्रा के बेघर यात्रियों" के, जो अपने जीवन को अनासक्त अनुभव और आनंद की प्राप्ति हेतु समर्पित कर चुके थे।
इन्हीं प्रेरित साधकों ने वाराणसी को अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव चुना। लेकिन गृहस्थों के लिए, वाराणसी को 'वर्जित क्षेत्र' माना गया (काशी खंड)।
वास्तव में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रुद्रवास में "घर बनाना" एक अपवित्र कार्य माना जाता था, क्योंकि कोई भी गृहस्थ वहाँ के रहस्यमयी साधकों से टकराव नहीं चाहता था, जिन्होंने अनंत काल से अपनी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए इसे उपयुक्त स्थान के रूप में सुरक्षित रखा था।
रुद्रवास में गृहस्थ जीवन को खतरनाक माना जाता था, क्योंकि वहाँ गणों और भूतों की अनियंत्रित उपस्थिति के कारण आए दिन संघर्ष भड़क उठते थे।
कोई भी गृहस्थ ऐसे अस्थिर और असुरक्षित स्थान को अपने निवास के लिए नहीं चुनता, जहाँ अज्ञात स्वभाव वाले लोग रहते हों।
यदि फिर भी वैदिक प्रवासियों ने इस 'भयानक' स्थान को उपनिवेश बनाने का प्रयास किया, तो हमें वैदिकों और गैर-वैदिकों के बीच निरंतर संघर्षों को ध्यान में रखना होगा।
इक्ष्वाकु वंश से लेकर गहड़वाल वंश तक के प्रवासी शासकों ने काशी-वाराणसी पर शासन किया, जब तक कि 1194 ईस्वी में गहड़वालों की अंतिम पराजय महमूद ग़ज़नी के हाथों नहीं हो गई।
बाद के समय में भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास (रामचरितमानस के रचयिता) ने अपनी विनय पत्रिका में वाराणसी के जीवन का एक अत्यंत नकारात्मक चित्रण किया। असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न अव्यवस्था और हिंसा ने लोगों को यहाँ बसने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया। काशी में रहना हमेशा जोखिम भरा माना गया। भूत-प्रेतों के डर, बाहुबलियों, धोखेबाजों और पाखंडियों के आतंक ने इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया।
इस बीच, स्वयं वैदिक समाज में भी बड़े बदलाव आ चुके थे। जब वे हप्त-सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मावर्त और कुषावर्त की अपनी बस्तियों से निकले, तो उनकी सांस्कृतिक परंपराएँ यजुर्वेद और ऋग्वेद के समय से काफ़ी बदल चुकी थीं। अथर्ववेद बाद में आया, और गृह्यसूत्रों का संकलन ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों के ऊपर किया गया।
शताब्दियों में जीवन और जीवनशैली बदल गई। संकीर्णता और रूढ़िवादिता ने धीरे-धीरे शैव समावेशिता और स्वीकृति की भावना को समाप्त कर दिया। अनुलोम, प्रतिलोम और नियोग विवाहों की स्वीकृति, तथा उनसे उत्पन्न संतान, ने समाज में जातिगत विभाजन और सामाजिक भेदभाव को और कठोर बना दिया।
प्रारंभिक वैदिक युग में विवाह का पारिवारिक संबंध के रूप में कोई कठोर नियम नहीं था। किन्तु बाद में बलपूर्वक विवाह भी स्वीकृत कर लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिंसक आक्रमण, बलात्कार और अपहरण की घटनाएँ इतनी आम हो गईं कि समाज को इन्हें स्वीकार करना पड़ा। समय बदल चुका था। शिव अब केवल एक आदिवासी देवता नहीं रहे, वे "देव-देव" (देवताओं के देवता) बन गए।
संस्कृतियों के बीच परस्पर घुसपैठ और आत्मसात की घटनाएँ बढ़ती गईं। वाराणसी ने इन्हें देखा, सहेजा और सहेजा। वाराणसी एक शाश्वत नगरी थी, है और रहेगी। अथर्ववेद और यजुर्वेद ने धीरे-धीरे कृषि, धातु, औषधि, राज्य-व्यवस्था, सैन्य-प्रशिक्षण, गृह-निर्माण और नागरिक कानूनों को स्वीकार करना शुरू किया। शुद्ध ऋग्वैदिक समाज के लिए यह अतीत से एक बड़ा विचलन था।
इस परिवर्तन का एक
साक्ष्य अथर्ववेद में इस प्रार्थना में मिलता
है—
"मेरे लिए दूध, घी,
शहद, भोजन,
सार्वजनिक भोज,
हल जोतना,
वर्षा, विजय,
समृद्धि, जौ,
चावल, तिल,
गेहूँ, लोबिया,
मसूर, बाजरा,
कदंब, तांबा,
सोना, चाँदी,
लोहा, पानी,
पशु, वृक्ष,
पर्वत—सब यज्ञ के माध्यम से संपन्न हों।"
वाराणसी का धीरे-धीरे "महाश्मशान" से "अविमुक्त" की अवस्था में संक्रमण केवल संघर्षों का ही नहीं, बल्कि महान सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का संकेत देता है। रुद्र की स्वीकृति महादेव और देव-देव के रूप में इन परिवर्तनों को प्रमाणित करती है।
आर्य दृष्टिकोण में भी व्यापक परिवर्तन आया। इसके परिणामस्वरूप, हिंदू धर्म नामक महान धार्मिक संस्था उभरी, जो एक समावेशी, सहिष्णु और उदार धर्म बन गई। हिंदू धर्म ने समस्त धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं को समाहित कर लिया। बलात् धर्म-परिवर्तन, राजनीतिक या परिस्थितिजन्य धर्मांतरण के विरुद्ध यह आज भी खड़ा है।
कोई वैष्णव शैव बन सकता था, कोई बौद्ध तांत्रिक बन सकता था, और इसके विपरीत भी, क्योंकि यह व्यक्तिगत आस्था का विषय था, न कि धर्मांतरण का।
यही कारण है कि धर्मांतरण का विचार उन लोगों के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था, जिन्होंने आपसी समायोजन और समझ को जीवन का मूल सिद्धांत माना था।
वाराणसी के नागरिकों में हुए इस क्रमिक परिवर्तन को समझना ही इस शाश्वत नगरी के मूल स्वरूप को जानने की कुंजी है। वाराणसी उन प्राचीन नगरों में से एक है, जिसने इतिहास के सबसे अधिक युगों को अपने पैरों के नीचे रौंदा है।
(इस संदर्भ में लेखक को स्मरण आता है कि भारत में प्रचलित "मुल्ला-कानूनों" के तहत किसी मुस्लिम का पुनः धर्मांतरण मृत्यु-दंड से दंडनीय अपराध था। यह कानून समावेशन और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देने में पूरी तरह विफल रहा।)
10.वाराणसी - सम्मोहक नगर
I
प्राचीन रुद्रवास और आनंदकानन अब अस्तित्व में नहीं हैं। इनके स्थान पर अब हमारे पास काशी-वाराणसी है।
पुराणों में वर्णित काशी-वाराणसी इससे भी अधिक प्राचीन होने का दावा करती है। जातकों में इसका उल्लेख मिलता है। वैदिक स्रोतों, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण (विदेघ माधव की कथा और सदानीरा की कथा), में काशी का उल्लेख (IV.1.10-17) मिलता है। इसका उल्लेख अथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा में भी पाया जाता है।
लेकिन सामान्यतः आर्यों ने इस स्थान से दूरी बनाए रखी, क्योंकि यहाँ वैदिक अग्नि को सम्मान नहीं दिया जाता था।
काशी का उल्लेख कौशीतकी, बृहदारण्यक, सांख्यायन और बौधायन श्रौतसूत्र, गोपथ ब्राह्मण, और यहाँ तक कि पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है, लेकिन वहाँ ‘काशी’ के स्थान पर ‘वाराणवती’ नाम का प्रयोग किया गया है।
यह हमारे अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। नगर के नाम के रूप में ‘काशी’ और ‘वाराणसी’ का उल्लेख बहुत बाद में हुआ।
क्या हम यह नहीं देख सकते कि ‘वाराणवती’ नाम स्वयं ही इस नगर के अस्तित्व और इसके विस्तार को वरुणा नदी के किनारे प्रमाणित करता है (और न कि गंगा के पश्चिमी तट पर, जैसा कि वर्तमान में दिखाई देता है)?
इस तथ्य से कई अनिवार्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
वैदिक लोगों ने यहाँ बसने से बचने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग अग्निहोत्र को प्रोत्साहित नहीं करते थे। उन्होंने पूरी तरह से अग्निहोत्र को अस्वीकार कर दिया (शत. ब्रा.)।
वैदिकों के लिए यह नगर वरुणा के तट पर स्थित था और पर्वतों की सीमा से दूर था। नगर का विस्तार और नगरीकरण उत्तर से दक्षिण की ओर हुआ। इसलिए, नगर के लिए वरुणा नदी गंगा से अधिक महत्वपूर्ण थी। इसीलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि ‘वाराणस्या’ नाम उस नगर के लिए अधिक उपयुक्त था, जो वरुणा के किनारे बसा था। उत्तरी आनंदकानन या रुद्रवास, जो वन से आच्छादित था, नवजात वाराणस्या या वाराणवती नगर से बहुत कम संबंध रखता था।
जैसे-जैसे नगर का विकास हुआ और यूनानी-शक संस्कृति की वास्तुकला और मूर्तिकला पर प्रभाव पड़ा, धीरे-धीरे मंदिरों और मूर्तिपूजक देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारंभिक वाराणस्या के मंदिर इन्हीं नए आवासीय क्षेत्रों के साथ निर्मित हुए, और शायद ही कभी केंद्रीय पर्वतों पर फैले। यह सीमित क्षेत्र हिंदू जीवन का केंद्र बन गया और इसे ‘अंतरवेदी’ या बाद में ‘विश्वेश्वरखंड’ के नाम से जाना जाने लगा।
पर्वतों के पूर्ववर्ती निवासी धीरे-धीरे दक्षिण और पश्चिम की ओर धकेल दिए गए।
मनुस्मृति में काशी का कोई उल्लेख नहीं है। क्या इसका अर्थ यह है कि इसे जानबूझकर अनदेखा किया गया, या फिर यह गैर-आर्यों के प्रति उपेक्षा का संकेत है? क्या यह पर्वतीय आदिवासियों के प्रति शत्रुता का परिचायक था? क्या यह आर्यों की अपने नगर ‘विदेह’ के प्रति प्राथमिकता और वाराणस्या के प्रति उदासीनता की शुरुआत थी? क्या यह गणों और देवों के बीच लगातार चलने वाले संघर्ष की जड़ थी? विदेह, एक आर्य उपनिवेश, काशी नगर का चिरस्थायी विरोधी बना रहा।
आर्यों ने आनंदकानन को वहाँ पाया, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी; उनके अग्निहोत्र यहाँ जलाए नहीं जा सकते थे, क्योंकि इसका भारी विरोध था (K. Kh., पुष्पदंत और दंडपाणि की कथाएँ)।
लेकिन इतिहास की धाराओं में प्रवाहित होते हुए, वाराणसी निरंतर विकसित होती रही और अंततः एक संपन्न नगर के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली।
उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक वाराणस्या नगर वरुणा नदी के तट तक ही सीमित था, जो धीरे-धीरे केंद्रीय पर्वतों और ज्ञानवापी तक विस्तारित हुआ।
बुद्ध ने काशी का उल्लेख किया है और दावा किया है कि वे कई बार वहाँ जन्मे थे। महावीर वास्तव में काशी-वाराणसी में जन्मे थे। यह नगर हड़प्पा काल से अब तक असीमित रूप से विकसित हुआ है।
आर्यों को यह पर्वतीय क्षेत्र पहले से बसा हुआ मिला और उन्होंने तुरंत इस सुंदर स्थल को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया, भले ही इसके लिए उन्हें प्राचीन, उग्र, अनार्य जनजातियों को विस्थापित करना पड़े। लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके (K. Kh.)।
यह कथा कि यह नगर शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ था, इसके निवासियों की विशिष्टता और उनकी आध्यात्मिक साधना को इंगित करती है। वे स्वयं को ‘संरक्षित’ मानते थे।
इसलिए, न तो महाकाव्य और न ही पुराण यह दर्शाते हैं कि वाराणसी भीड़भाड़ वाला नगर था। इसके विपरीत, सभी उल्लेखों में यह कहा गया है कि मन्दाकिनी और गोदावरी के पार का क्षेत्र वनों से आच्छादित था और झरनों से सिंचित था, जिसे आनंदकानन कहा जाता था। यह वास्तव में एक मनमोहक आश्रय स्थल था, जहाँ साधक शांति और एकांत में निवास कर सकते थे। इसे प्रेमपूर्वक ‘रुद्रवास’ कहा जाता था, जो कि नगरीय वाराणसी से कई शताब्दियों पूर्व अस्तित्व में था।
वह काशी भी अब लुप्त हो चुकी है। आनंदकानन के स्थान पर आज हमारे सामने एक परिवर्तित, जनसंख्या से भरपूर नगर खड़ा है। फिर भी, यह हमें काशी, वाराणसी, या बनारस जैसे भ्रामक नामों के माध्यम से भ्रमित करता है।
कुछ अन्य अर्द्ध-ऐतिहासिक संदर्भ काशी की अत्यंत प्राचीनता की ओर संकेत करते हैं। पुराणों में एक राजा काश (लगभग 3000 ईसा पूर्व, कुरुक्षेत्र युद्ध के आधार पर गणना) का उल्लेख मिलता है। उनके पुत्र का नाम ‘काशिराज’ था, जिनकी पुत्री गंदिनी का विवाह यादव वंश के स्वफल्क से हुआ। स्वफल्क के पुत्र अक्रूर की मृत्यु कृष्ण वासुदेव के हाथों पौंड्र वासुदेव के विरुद्ध युद्ध में हुई।
काशी का एक अन्य व्युत्पत्ति-सिद्ध व्याख्या ‘कस’ मूल धातु से की जाती है, जिसका अर्थ है प्रकाश। इस प्रकार, काशी को ‘प्रकाश का नगर’ कहा गया। (K. Kh., XXVIV)
हालाँकि, पुराण-कवियों की ये व्याख्याएँ बुद्धिमत्ता और चतुराई से भरी प्रतीत होती हैं, फिर भी वे अधिकतर बाद की व्याख्याएँ लगती हैं।
पुराण इस प्रकार की साहित्यिक युक्तियों से भरे पड़े हैं।
जो भी हो, हमारे पास काशी-वाराणसी का यह नगर है, जिससे हम इसके अतीत को खोजने और पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं।
लेकिन क्या यह संभव है कि हम ‘बीते दिनों का प्रकाश’ वापस ला सकें?
हम पुनः वाराणसी को खोज सकते हैं और इसकी खोई हुई भव्यता को देख सकते हैं, जैसे कि संग्रहालयों में रखी कलाकृतियाँ हमें एथेंस, पोम्पेई, क्नोसस, पर्सेपोलिस, या टेनोचिट्लान (मेक्सिको) की खोई हुई भव्यता को देखने का अवसर देती हैं।
वाराणसी - सम्मोहक नगर
II
हमारे लाभ के लिए, क. ख. ने पहले ही वाराणसी के भू-लेख का विभाजन कर दिया है। हम इससे लाभ उठा सकते हैं। अनादि काल से वाराणसी की यात्रा करने वाले करोड़ों श्रद्धालु तीर्थयात्रियों ने क. ख. द्वारा निर्धारित तीर्थ मार्गों से लाभ प्राप्त किया है।
वाराणसी में तीर्थ स्थल वास्तव में वैदिक युग के महान ऋषियों की आध्यात्मिक स्मृतियों में प्रतिष्ठित स्थान हैं। वाराणसी के सामान्य वन, सामान्य सरोवर और कुएँ अर्ध-दैवीय व्यक्तित्वों की महान विभूतियों को स्मरण कराते हैं, जिन्होंने इन पवित्र पर्वतों को अपना निवास स्थान बनाया।
साधारण भूमि महात्माओं के गुणों और बलिदानों से अमर हो जाती है। वाराणसी में अगस्त्य, कर्दम, मार्कण्डेय, हरिश्चंद्र, कपिल, दत्तात्रेय, गौतम, दुर्वासा और कई अन्य महान आत्माओं ने अपनी छाप छोड़ी है।
लोकप्रिय मान्यता के विपरीत, वाराणसी के तीर्थयात्रा स्थलों और पवित्र स्थानों का संबंध किसी चमत्कारी दैवीय प्रकटियों से नहीं है। पुराणों की कथाएँ मात्र कथाएँ हैं और उन्हें प्रतीकात्मक अथवा रूपक भाषा के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। अधिकांश पवित्र स्थल मानवीय तपस्या और बलिदानों से जुड़े हुए हैं। वाराणसी में ऐसे कई पावन स्थल रहे हैं।
आज केवल नाम ही हमें स्मरण कराते हैं। अगस्त्य मुनि के आश्रम, एकमात्र ध्रुव के आश्रम, भैरव दत्तात्रेय के स्थान, अथवा महान व्यास के स्थल आज भी हमारे सम्मुख खड़े हैं, जब हम इन पावन धूलिकणों पर खड़े होते हैं।
आज तक महान पुण्यात्माओं के नाम पर स्मारक बनाना वाराणसी की एक स्वस्थ परंपरा रही है। इस परंपरा में नवीनतम जोड़ तुलसीदास, अघोरी केनाराम, तैलंग स्वामी, स्वामी भास्करानंद, संत रामकृष्ण परमहंस, यहाँ तक कि हमारे ही युग की संत माँ आनंदमयी और रहस्यवादी अवधूत ठाकुर सीताराम ओंकारनाथ हैं।
वाराणसी में तीर्थयात्राएँ हिंदू भारत की संस्कृति और विरासत की निर्देशिका के रूप में कार्य करती हैं।
हम वाराणसी के विभिन्न खंडों - ओंकार, विश्वनाथ और केदार खंड से परिचित हैं।
एक अन्य विभाजन, जो शास्त्रों में उल्लिखित है, उनके लिए व्यवस्थित किया गया है जो प्रतिदिन, समय-समय पर, या वार्षिक रूप से सबसे पवित्र स्थलों की परिक्रमा करना चाहते हैं। ये तीन खंड इस प्रकार हैं: (1) वाराणसी, (2) अविमुक्त, और (3) अंतरगृह अथवा विश्वनाथ। इनका उपयोग तीर्थयात्रा के लिए परिक्रमा मार्ग के रूप में किया जाता है।
पंचक्रोशी परिक्रमा आनंदकानन की प्राचीन सीमाओं के चारों ओर निर्धारित की गई है। इसे पाँच दिनों में पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पर्वतों के चारों ओर जाती है, जिसकी पूर्वी सीमा गंगा है। लेकिन पंचक्रोशी तीर्थयात्रा वाराणसी के चारों ओर होती है, जिसमें गंगा, असि और वरुणा इसकी सीमाएँ बनाते हैं।
इससे पता चलता है कि वाराणसी एक संकुचित नगर था, लेकिन पश्चिम और दक्षिण में इसका वन क्षेत्र विस्तृत था।
वर्ष में केवल एक बार, शीतकाल और आगामी वसंत के बीच की एक निश्चित अवधि में, यह परिक्रमा श्रद्धालुओं द्वारा पाँच दिनों की यात्रा में पूरी की जाती है, अन्यथा सवारी, पालकी या पशुओं पर की जाती है।
अविमुक्त या मध्येश्वर परिक्रमा एक दिन में संपन्न होती है। यद्यपि आजकल यह दुर्लभ हो गया है, फिर भी कुछ श्रद्धालु इसे प्रतिदिन करने का संकल्प लेते हैं।
अंतरगृह परिक्रमा, हालाँकि, वाराणसी के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों को समेटे हुए है और हजारों श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। मध्येश्वर में कुछ प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मंदिर शामिल हैं।
अंतरगृह का क्षेत्र, जिसे हम अपनी वाराणसी की खोई हुई विरासत की खोज हेतु गहराई से अन्वेषण करने वाले हैं, एक सघन और अब भी जीवंत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बिखरे प्रमाण, यद्यपि समय-समय पर विनाश, चोरी और प्रशासनिक अराजकता के कारण पहचानने योग्य नहीं रह गए हैं, फिर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यह क्षेत्र सूचनाओं का भंडार है और हमारी खोज के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
यही क्षेत्र (अंतरगृह-मध्येश्वर) खोई हुई वाराणसी का हृदयस्थल है। इसे खोजकर, हम वाराणसी को पुनः खोज लेंगे और समझ सकेंगे।
इस क्षेत्र का एक नक्शे के आधार पर अन्वेषण स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करेगा कि रुद्रवास का विस्तार हुआ और इसने 'हृदयस्थल' - अंतरगृह को प्रभावित किया, जो मूल रूप से रुद्रों का आधार था, और जहाँ से उन्हें विस्थापित कर दिया गया तथा पश्चिम और दक्षिण की दलदली भूमि के किनारों तक सीमित कर दिया गया।
यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि वाराणसी का कोई अन्य क्षेत्र इससे अधिक विनाशकारी परिवर्तन से नहीं गुजरा। पुरानी वाराणसी को उन लोगों की अदूरदर्शिता ने परिवर्तित कर दिया, जिन्होंने अपने समय की घटनाओं पर शासन किया। फिर भी यह क्षेत्र पुजारियों, गाइडों और उन दलालों द्वारा केंद्र में रखा गया है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भोजनालयों के आसपास मंडराते हैं, जिससे यह तथाकथित वाराणसी पर्यटन का केंद्र बन गया है।
III
कोई भी निर्दोष यात्री, श्रद्धालु या दर्शक यह संदेह नहीं करेगा कि वाराणसी की यात्रा के दौरान, पेशेवर गाइडों की बदौलत, उन्हें असली अनाज के स्थान पर भूसा, सोने के स्थान पर सस्ता धातु, और असली रत्नों के बदले कृत्रिम आभूषण बेचे जा सकते हैं। प्रचलित गाइड, जो न तो इतिहास की परवाह करते हैं और न ही सटीकता की, आमतौर पर वास्तविक जिज्ञासु को गुमराह कर देते हैं। फिर भी, वाराणसी-यात्रा के सबसे विश्वसनीय संरक्षक चयनित पंडित-गाइड या पुरोहित-गाइड होते हैं। इन्हें अत्यधिक सावधानी से चुनना आवश्यक है।
नक्शे पर एक अच्छी नज़र डालने से स्पष्ट होगा कि रुद्रवास अंतरगृह के केंद्र से बहुत आगे तक फैला हुआ था और इसे पूरी तरह घेर लिया था। मूल रूप से, रुद्र इस क्षेत्र में निवास करते थे। लेकिन उन्हें विस्थापित कर दिया गया और वे बाद में दलदली भूमि और समतल क्षेत्रों तक सीमित रह गए।
इस क्षेत्र में प्राचीन आवासों का कोई अवशेष शेष नहीं है। आम धारणा के विपरीत, सबसे बड़ा नुकसान मंदिरों के विनाश से नहीं हुआ, क्योंकि ये वैसे भी गुप्त युग के बाद निर्मित हुए थे। बल्कि, सबसे गंभीर क्षति वाराणसी के ऐतिहासिक स्थलों, उसकी नदियों, सरोवरों, झीलों और विशेष रूप से प्रसिद्ध घाटियों को पूरी तरह से मानचित्र से हटा देने से हुई। ये मंदिरों से भी पहले अस्तित्व में थे, क्योंकि किसी भी मंदिर का निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी से पहले नहीं हुआ था।
वाराणसी को इस तरह से नष्ट करने का कार्य किसने किया? इस बर्बरता के लिए कौन उत्तरदायी थे? इस प्रश्न का उत्तर हमारे अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वाराणसी को अभी भी पूरी तरह से खोजा जाना बाकी है।
अधिकांश तालाब और जलाशय, अधिकांश नदियाँ सदियों की विनाश और उपेक्षा की परतों के नीचे दबी हुई हैं। सरोवर और झीलें, जो प्राकृतिक और मौसमी वर्षा जल से भरती थीं, अब सूख चुकी हैं, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से पुनः भरने का अवसर नहीं मिला।
पूर्ण विनाश के बावजूद, विभिन्न संकेतक अब भी शोधकर्ताओं को उन शास्त्रीय स्थलों का पता लगाने में सहायता करते हैं, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया गया है।
अत्यधिक महत्व के स्मारक अभी भी खोजे जा सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग उनके अस्तित्व को समझते हैं। वे खोए हुए स्मारक, मंदिर और झीलें, जिन्हें गंभीर रूप से प्रभावित किया गया है, आमतौर पर पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल नहीं होतीं। यदि वे अस्तित्व में हैं, तो वे कुख्यात रूप से संकरी और भीड़भाड़ वाली गलियों में छिपे हुए हैं। प्राचीन वाराणसी इन गलियों के भीतर ही अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, मोटर योग्य सड़कों से दूर।
वह समय अधिक दूर नहीं जब ये अल्प प्रमाण भी धूल में विलीन हो जाएँगे; जब अन्य संरचनाएँ अतीत को पूरी तरह से दफन कर देंगी। वाराणसी मृत हो चुकी है। यहाँ तक कि इसकी राख भी अनुचित शहरी प्रशासन द्वारा मिटाई जा रही है। (गड़ुरेश्वर, मानसरोवर, ईशरगंगी जैसे क्षेत्रों का पतन इसका उदाहरण है।)
IV
वाराणसी में पर्यटकों को केवल लोकप्रिय, प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मंदिरों के दर्शन के लिए घुमाया जाता है। मंदिरों के भीतर छिपे अनगिनत देवी-देवता, जो संकरी गलियों और कठिन पहुँच वाले स्थानों में स्थित हैं, तब तक उजागर नहीं होते जब तक कि कोई आग्रही यात्री दृढ़ता से उनकी माँग न करे। धार्मिक निवासी, हालांकि, इन स्थानों को जानते हैं और बिना किसी गहरी विद्वता की खोज में वहाँ जाते हैं। वाराणसी को पूरी तरह से जान पाना असंभव है।
असंख्य मंदिरों की यात्रा करना अत्यंत उबाऊ हो सकता है। एक ही प्रकार की भिक्षुकों, साधुओं, साँड़ों, गंदे और भीड़भाड़ वाले रास्तों, धर्म के नाम पर ठगने वालों, अनैतिक दलालों, चालाक गाइडों और एक तांबे के सिक्के के लिए ललायित भूखे चेहरों के बीच भटकना हर किसी के लिए रुचिकर नहीं होता। ये सभी अपने-अपने तरीकों से एक श्रद्धालु की सरल आस्था पर जीवन यापन करते हैं।
जो लोग गहरी जानकारी चाहते हैं, वे अंततः यह पाते हैं कि स्वयं गाइड को भी कुछ ज्ञात नहीं। अंततः, ऐसी यात्रा विद्वानों और जिज्ञासुओं दोनों को समान रूप से निराश और शायद खिन्न भी कर देती है।
वास्तव में, ऐसा होना आवश्यक नहीं था। वाराणसी हमेशा से एक अत्यंत रोचक और लाभकारी स्थान रही है। वाराणसी का आंतरिक आत्म हमेशा से शांति में स्थित रहा है।
शताब्दियों पहले, यह केवल संतों और साधुओं से भरे नीरस मंदिरों का ही नगर नहीं था, बल्कि शांत वन, ठंडी जलाशय, सुरम्य वातावरण और सबसे बढ़कर संतों की शांति-युक्त संगति ने मनुष्यों को वृक्षों से घिरी उस रमणीय वाराणसी की ओर आकर्षित किया था।
वह वाराणसी कहाँ लुप्त हो गई? वह कहाँ चली गई?
V
हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो स्थान अब 'मंदिरों' के रूप में प्रसिद्ध हैं, वे मात्र व्यक्तिगत या सामुदायिक अहंकार, वैभव, शक्ति और नाम की स्थायित्व की मानवीय दुर्बलता के विस्तार मात्र हैं।
पवित्र स्थलों के चारों ओर दीवारें खड़ी करके और कुछ लोगों को उनके भीतर प्रवेश से वंचित करके, सत्ता में बैठे लोग मूल रुद्रवास के मुक्त और खुले समाज को बनाए रखने में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं।
प्राचीन वाराणसी एक स्वतंत्र स्थान था, जो किसी के लिए भी खुला था, बिना किसी प्रतिबंध, अवरोध या अधिकार के।
आज जो मंदिर हम देखते हैं, वे बाद की कृतियाँ हैं, जिन्हें राजाओं, सम्राटों, पुजारियों, विधि-निर्माताओं और धनवान व्यापारियों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। और यह सब धर्म के नाम पर हुआ।
हमने देखा है कि मंदिर-संस्कृति वाराणसी की मूल संस्कृति नहीं थी, जैसा कि बेबीलोन, उर, पर्सेपोलिस, अमारना, लक्सर, एथेंस, क्नोसस और नीनवे में था।
वेदों में मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। न ही रामायण और महाभारत में मंदिरों का कोई वर्णन है। हम किसी भी मंदिर के बारे में यूनानियों, शकों, गांधारों और विशेष रूप से सम्राट कनिष्क से पहले नहीं सुनते, जो स्वयं एक विदेशी शासक थे।
ईसाई युग से पहले प्रायद्वीपीय भारत में कोई मंदिर और न ही कोई नक्काशीदार मूर्तियाँ थीं। जातक कथाओं और महाकाव्यों के अध्ययनकर्ता अक्सर चैत्य, स्तूप, विहार, वापी (तालाब), तीर्थ, कुंड (जलाशय) और कूप (कुएँ) पाते हैं; लेकिन वे न तो नक्काशीदार मूर्तियों के बारे में सुनते हैं और न ही पत्थर से बने मंदिरों के बारे में, जब तक कि फा-हियान और ह्वेनसांग ने उनका उल्लेख नहीं किया।
मंदिर माता की उपासना करने वालों या शिवलिंग की पूजा करने वालों के लिए अज्ञात थे।
यह हमें एक नई दिशा में सोचने और एक नई यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करता है।
हमारा उद्देश्य प्राचीन वाराणसी की खोज है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, हम उस वाराणसी के संभावित पुनर्निर्माण और पुनर्वास का प्रयास करेंगे, जो भारत की गौरवशाली धरोहर थी। वह वाराणसी समृद्ध पूर्वी सभ्यता का केंद्र थी। इसके प्रसिद्ध तपोवनों, मंदिरों और बाजारों में राजकुमार, पुजारी, संन्यासी, तपस्वी, विद्वान, कवि, दार्शनिक और संगीतज्ञ आकर्षित होते थे।
वाराणसी का कौन सा जादू संतों और विद्वानों को आकर्षित करता था? वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, कबीर, रामानंद, गोरखनाथ, रामकृष्ण, दयानंद और यहाँ तक कि माँ आनंदमयी भी वाराणसी की ओर क्यों आकर्षित हुए? भारत के सर्वश्रेष्ठ और महानतम लोग हमेशा वाराणसी में रहने के लिए उत्सुक रहे। यह चिरंतन तीर्थयात्रा, जो ब्रह्मांडीय खोज की ओर प्रेरित करती है, आज भी कई रहस्यों को उजागर कर सकती है जो हमें चकित कर दें।
प्राचीन वाराणसी और गंगा थी; और आज भी वाराणसी और गंगा हैं। मंदिर और उनकी सजावट बाद में आई, बहुत बाद में।
हम मंदिरों की काल-रेखा को पार करके उस खोई हुई वाराणसी को पुनः खोजने के इच्छुक हैं, जहाँ लिंगम, वन, तालाब, झीलें, नदियाँ और कुएँ थे।
इस संदर्भ में, हम हिंदू धर्म के आध्यात्मिक तत्वों या मंदिरों और पुजारियों की पवित्रता पर किसी भी चर्चा से खुद को सावधानीपूर्वक दूर रखेंगे।
11.परिवर्तित होता नगर
I
यह उल्लेख किया गया है कि वाराणसी को तीन खंडों में विभाजित किया गया था: विश्वेश्वरखंड, ओंकारखंड और केदारखंड। हमारे पास इस संपूर्ण पवित्र नगर के भू-भाग की एक स्पष्ट धारणा है, जिसमें ओंकारखंड को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र के चारों ओर सबसे प्रमुख पवित्र मंदिर और सबसे प्रतिष्ठित घाट स्थित थे।
वाराणसी का शेष भाग, जो पहाड़ियों से परे था (अर्थात वर्तमान बंगालीटोला गली के पश्चिम में, चेतगंज और जगतगंज मार्गों के पार, केदार और हरिश्चंद्र घाट से लेकर खोजवा और जी.टी. रोड तक), वास्तव में पंचक्रोशी मार्ग के चारों ओर फैला हुआ था और विशाल वन क्षेत्रों से ढका हुआ था। यहाँ-वहाँ इस क्षेत्र में कई जलाशय स्थित थे, जिन्हें कुंड, तालाब, पोखर या पुष्करणी के नाम से जाना जाता था, जैसे रेवतीकुंड, वेणीकुंड (बेनियातालाब), लहरियातालाब, ईश्वरगंगीतालाब, पिशाचमोचनतालाब, मिसिर पोखरा, लक्ष्मी कुंड आदि। इनमें से कुछ 300-400 एकड़ तक फैले हुए थे। मंदाकिनी झील एक वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में विस्तृत थी, और मत्स्योदरी झील के साथ मिलकर और भी अधिक। छोटे जलाशयों की संख्या बहुत अधिक थी।
दुर्भाग्य से, इनमें से अधिकांश जलाशय अब मृतप्राय हैं, जैसे मिसिर पोखरा। शहरीकरण का विस्तार एक ऐसा दैत्य है जो सब कुछ निगल जाता है और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। रेवती पुष्करणी (रेउर तालाब), मिसिर पोखरा या महान मंदाकिनी तालाब का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है।
इतने अधिक जलाशयों की उपस्थिति इस नगर की भू-संरचना की दो प्रमुख विशेषताओं को दर्शाती है। पहली, भूमि की ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर थी; और दूसरी, वास्तविक वन क्षेत्र अपेक्षाकृत विरल बसा हुआ था, या फिर वहाँ स्थानीय लोग रहते थे जो आर्यों की पहुँच से दूर रहना पसंद करते थे। इस क्षेत्र की एक अन्य विशेषता इसकी असीमित हरियाली थी। आधुनिक वाराणसी के अधिकांश भाग कभी घने वनों से ढके हुए थे।
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों (1920-1930) तक संकटमोचन, भैरवनाथ, और शंकर मठ जैसे क्षेत्र वनस्पतियों से आच्छादित थे और यहाँ संन्यासियों के कुटीर स्थित थे। अब इस क्षेत्र का 'विकास' कर दिया गया है।
हालाँकि, ओंकारखंड की स्थिति भिन्न थी, अर्थात यह भूमि वरुणा नदी के दोनों किनारों से लगी हुई थी, विशेष रूप से इसके दक्षिणी तट पर, मंदाकिनी तालाब और मत्स्योदरी तक फैली हुई थी।
वाराणवती, वाराणस्या या वाराणसी इसी क्षेत्र में स्थित थी। बाद में लिंग पुराण में शिव माता पार्वती से कहते हैं कि वाराणसी असि और वरुणा के बीच स्थित है। लिंग पुराण की यह व्याख्या महत्वपूर्ण है। असि और वरुणा के बीच का क्षेत्र आनंदकानन था, जो शिव, भैरव और पाशुपत संप्रदाय के संतों का प्रिय आश्रय स्थल था। इसलिए, वास्तव में यह क्षेत्र शिव का प्रिय निवास था, न कि केवल वरुणा नदी के सामने बसा हुआ नगर।
स्कंद पुराण और विशेष रूप से लिंग पुराण 'मध्येश्वर' नाम को विशेष महत्व देते हैं, जहाँ 'मध्य' का अर्थ 'बीच' है। यह देवता संभवतः नगर के 'मध्य' में रक्षक के रूप में कार्य करता था।
इसलिए, वाराणस्या नगर का प्रमुख भाग था; आनंदकानन असि और वरुणा के बीच स्थित शिव का निवास था; और इन दोनों के मध्य मध्येश्वर स्थित था। (मत्स्योदरी का अर्थ भी मछली के आकार के मध्य भाग से जुड़ा है।)
इस मान्यता के अनुसार, कृतिवास प्रमुख देवता थे, और कृतिवासेश्वर (आधुनिक आलमगीरी मस्जिद, औसानगंज के पास) से प्रारंभ होकर, वास्तविक वाराणवती या वाराणसी क्षेत्र कुछ मीलों तक फैला था, जिसमें मध्येश्वर केंद्र में स्थित था।
लेकिन इन सभी बातों के बावजूद, पहाड़ियाँ और दक्षिण की ओर फैले वन शिव के प्रिय स्थान बने रहे (लिंग पुराण)।
मोतीचंद्र अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि यह याद रखना बुद्धिमानी होगी कि वरुणा के उत्तरी तट पर भी नगर का विस्तार कई मीलों तक फैला हुआ था। यदि इस तथ्य को स्वीकार किया जाए, तो पुराणों में वर्णित नगर की सीमाएँ अधिक यथार्थपरक प्रतीत होती हैं।
वरुणा के उत्तरी तट पर नगर की उपस्थिति सारनाथ की स्थिति से भी स्पष्ट होती है, जहाँ से बुद्ध अक्सर नगर के लोगों को उपदेश देने आते थे।
आज भी, वाराणसी और गाजीपुर के बीच के मार्ग पर कई छोटे नगर और गाँव मिलते हैं, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ संपन्न व्यापार हुआ करता था, जिसने वाराणसी को 'जितवारी' (जहाँ व्यापारी सदैव लाभ कमाता है) नाम प्रदान किया था (अष्टाध्यायी 4.3.72)।
जातकों में भी यह संकेत मिलता है कि नगर का विस्तार वरुणा के दोनों किनारों तक था। कई स्थानों जैसे सैदपुर, कैथी, पोटली और वैनरत का अस्तित्व आज भी उन समृद्ध बस्तियों की याद दिलाता है, जो मृगदाव, कपिलधारा, मार्कण्डेय और वरुणा के बीच स्थित थीं। इनमें से वैनरत पुरातात्विक महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अवशेष वाराणसी के उत्तरी तट के परे विस्तार को प्रमाणित करते हैं।
अब हम पुराणों में वर्णित इस पवित्र नगर के भू-भाग का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करेंगे।
इसके लिए हमें कुछ मानसिक अनुशासन अपनाना होगा और वर्तमान नगर के स्वरूप को पूरी तरह से अपनी कल्पना से मिटाना होगा।
हम इस कार्य को वर्तमान उपलब्ध स्थलों और संकेतों के आधार पर करेंगे।
सबसे प्राचीन उपलब्ध अभिलेखों में वाराणसी को तीन प्रमुख पहाड़ियों (शिव के त्रिशूल) के चारों ओर निर्मित नगर के रूप में दर्शाया गया है। आधुनिक नगर-निर्माण की भारी विनाशलीला के कारण अब ये पहाड़ियाँ स्पष्ट रूप से पहचान में नहीं आतीं। लेकिन यह तथ्य बना हुआ है कि प्राचीन वाराणसी वास्तव में इन्हीं तीन पहाड़ियों के चारों ओर स्थित थी।
इन पहाड़ियों के अवशेष, जो अब भी अपने अस्तित्व की कहानी कहते हैं, पूर्व की ओर नदी, पश्चिम की ओर ढलानों और घाटियों से मिलते हुए दलदली भूमि और जंगलों तक फैले हुए हैं।
इन स्थलों का सूक्ष्म अध्ययन एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है।
प्राचीन वाराणसी की खोई हुई नदियों और तालाबों का पता भी इन पर्वतीय संरचनाओं के माध्यम से लगाया जा सकता है। इस प्रकार, जो अब अस्तित्व में नहीं है, उसे विद्यमान संकेतों की सहायता से पुनः स्थापित किया जा सकता है।
इस प्रकार, वाराणसी को पुनः खोजने के हमारे प्रयास में, 'खोई हुई पहाड़ियों' के ये चिह्न हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होंगे और हमें महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करेंगे।
परिवर्तित होता नगर
II
सामान्य रूप से, पहले वर्णित प्राचीन तीन विभाजन, तीन पहाड़ियों और उनके विस्तार को स्पष्ट करते हैं।
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय पहाड़ी है, जो अब त्रिलोचन से दशाश्वमेध तक के क्षेत्र को (पूर्व की ओर) और कबीरचौरा से गोदौलिया तक (राजादरवाजा, चेतगंज और बेनिया सहित पश्चिम की ओर) कवर करती है। यह क्षेत्र वाराणसी के सर्वोच्च स्थल को दर्शाता है और इसमें चौक भी शामिल है।
इस पहाड़ी का वाराणसी में योगदान दो धाराओं के रूप में मिलता है। इनमें से एक दक्षिण की ओर बहती थी और मिसिर पोखरा की दलदली भूमि से निकलने वाली धारा से मिलती थी। फिर यह पूर्व की ओर मुड़ती थी और गोदावरी जलमार्ग को पोषित करती थी, जो प्रयाग घाट पर गंगा से मिलती थी।
दूसरी धारा, जिसे अब भी बुलानाला (नाला-धारा) के नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी सरोवर में प्रवाहित होती थी। ये दोनों धाराएँ वनाच्छादित घाटियों से होकर बहती थीं, जहाँ कभी-कभी आश्रमवासियों के कुटीर बसे होते थे।
आधुनिक वाराणसी की सबसे व्यस्ततम सड़क के किनारे स्थित दुकानों की कतारें अब इस पहाड़ी, जलधाराओं, मंदिरों और वनों के अस्तित्व की कोई याद नहीं दिलातीं।
इन जलाशयों और आसपास के मंदिरों के मौन साक्षी के रूप में आज भी एक मध्यम आकार का तालाब, देवी मंदिर और राम मंदिर विद्यमान हैं।
आधुनिक स्वरूप में यह क्षेत्र यातायात की अव्यवस्था और भ्रम उत्पन्न करता है। इसका कारण यह है कि यह महत्वपूर्ण क्षेत्र कभी आनंदकानन का शिखर हुआ करता था और इसलिए यह प्राचीन काल में ऋषियों और मुनियों के लिए सबसे प्रिय स्थान था। उन दिनों यहाँ वाणिज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। कोई भी शत्रु इसे आक्रमण या कब्जे का लक्ष्य नहीं बनाता था, जब तक कि इसके शीर्ष पर कोई मंदिर न बनाया गया हो।
कालांतर में, यह क्षेत्र सहायक मंदिरों, पूजास्थलों, मठों और आश्रमों का एक विशाल केंद्र बन गया। यहाँ संत, विद्वान, ऋषि, साथ ही मंदिर सेवक और पुजारी निवास करते थे।
जहाँ तीर्थयात्री होते हैं, वहीं व्यापार पनपता है; और जहाँ व्यापार होता है, वहाँ भीड़ उमड़ती है।
विनाश की अनेक घटनाओं और उसके परिणामस्वरूप आए परिवर्तनों के बावजूद, इस क्षेत्र की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। जिस प्रकार किसी विशाल भँवर की केंद्रीय शक्ति तैरते हुए टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार वाराणसी में अनेक विनाशों के बाद भी, सार्वजनिक ध्यान और व्यापार इसी क्षेत्र में केंद्रित रहा।
इस क्षेत्र के आसपास युगों से मंदिर, पूजास्थल, धर्मशालाएँ, कारवाँसराय और यहाँ तक कि वैदिक और लौकिक अध्ययन के विद्यालय फलते-फूलते रहे।
वाराणसी के प्रसिद्ध संगीतकार, गायक, नर्तक और कलाकार मंदिर चौक के आसपास निवास करते थे।
हर बार जब विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया, तब इसका पुनर्निर्माण होता रहा। जब भी शासक सत्ता शिथिल हुई या सत्ता कमजोर पड़ी, तो उत्साही भक्तों ने इस क्षेत्र को पुनः खड़ा करने का प्रयास किया। यहाँ हमेशा धन उपलब्ध रहा। विनाश का अंत नहीं था, और पुनर्निर्माण का भी कोई अंत नहीं था। धार्मिक उत्साह ने अक्सर तलवार के खिलाफ आग, पीड़ा के खिलाफ समर्पण, स्मृति के खिलाफ आशा को प्रतिस्थापित किया।
यहाँ एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया जा सकता है। भारत में (सौराष्ट्र के सोमनाथ को छोड़कर) कोई अन्य नगर वाराणसी जैसा बार-बार कट्टरपंथियों के हमलों का शिकार नहीं हुआ। अनेक विध्वंसों के बाद, विश्वनाथ मंदिर बार-बार पुनर्निर्मित हुआ।
परंतु प्रश्न यह उठता है कि कृतिवास, अविमुक्त, ओंकार, कालेश्वर और मध्येश्वर जैसे प्रसिद्ध मंदिर, जिनकी पुराणों में विश्वनाथ से अधिक प्रशंसा की गई है, कभी पुनर्निर्मित क्यों नहीं किए गए? और विश्वनाथ मंदिर को इतना अधिक महत्व कैसे मिला?
हमें ज्ञात है कि पहाड़ियाँ, जो नगर-आधारित मंदिरों से भिन्न थीं, तीन विशेषताओं से परिपूर्ण थीं: (1) वे ऋषियों का आश्रय स्थल थीं, (2) वहाँ गणों और रुद्रों का निवास था, (3) वे घने वनों से आच्छादित थीं।
पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित शिवलिंग एक स्वयंभू लिंग था (पूर्व-आर्य कालीन चिह्नित पूजास्थल, जिसे शास्त्रों के अनुसार 'प्रतिष्ठित' नहीं माना जाता था) और यह मूल निवासियों द्वारा पूजित था।
वास्तव में, 'सच्चे' ब्राह्मण इस 'भैरव' देवता के प्रसाद को ग्रहण करने से हिचकते थे। भक्तों को 'जाति-विहीन' माना जाता था और वे 'वैदिक अग्नि' को बनाए रखने के अधिकार से वंचित थे (शतपथ ब्राह्मण)।
इसलिए, जब पहाड़ियों पर स्थित मंदिर और पूजास्थल नष्ट किए गए, तो गण, रुद्र और भैरव के भक्तों ने शीघ्र ही पुनः इकट्ठा होकर अपनी प्रार्थनाएँ जारी रखीं।
वे निर्धन थे और शास्त्रीय बाधाओं से मुक्त थे, इसलिए भैरव-विश्वनाथ की आत्मा कभी नष्ट नहीं हुई। जब संपन्न नगर-मंदिर उपेक्षित हो गए, जब नगर के धनवान लोग असफल हो गए, तब भी वनवासी अपने आराध्य को बचाने में सफल रहे, भले ही उन्हें स्थान बदलना पड़ा या नए मंदिर में रुचि छोड़नी पड़ी।
आज, जब अन्य प्रसिद्ध देवता उपेक्षा के कारण लुप्त हो चुके हैं, तब भी वनवासियों द्वारा पूजित 'मूल' स्वयंभू देवता अपनी महिमा बनाए हुए हैं।
हमें इस बिंदु पर पुनः लौटना होगा।
भक्तों की स्मृतियाँ, जैसे पुराने प्रियजन की यादें, भारी विनाश के बाद भी केवल परिचित क्षेत्र से जुड़कर राहत और विश्वास पाती हैं।
यह अचरज की बात नहीं है। संकट में फँसा नाविक भी बहते हुए मलबे को पकड़कर राहत महसूस करता है। जो लोग बलपूर्वक धर्मांतरण के शिकार हुए, उन्होंने भी विनाश के बाद इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज चौक, दालमंडी, बेनिया, जैतपुरा, अलईपुरा और मदनपुरा में बड़ी संख्या में वे धर्मांतरित लोग बसे हुए हैं।
मदनपुरा का उल्लेख जिनप्रभा सूरी (1350 ईस्वी) के 'विविध तीर्थकल्प' (VTK) में एक मुस्लिम बस्ती के रूप में किया गया है। यह क्षेत्र 1340 ईस्वी से, जब मुहम्मद तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर था, हिंदू धर्मांतरित समुदाय से भरा हुआ था।
यद्यपि वे धर्मांतरित हो गए थे, फिर भी वे अपने पुराने निवास स्थानों से जुड़े रहे।
स्मृति की शक्ति एवं मूल प्रवृत्तियाँ हमेशा सक्रिय रहती हैं। बाहरी दबाव उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते।
वाराणसी सदियों से विनाश और पुनर्निर्माण के इस चक्र से गुजरती रही है। यह नगर सात शताब्दियों तक पतन, विघटन और अराजकता से हिलता रहा।
इस पतन की गवाही देने वाले कुछ बचे-खुचे बस्तियाँ आज भी अस्तित्व में हैं।
यह क्षेत्र हमें वाराणसी की खोई हुई महिमा और विश्वनाथ मंदिर की याद दिलाता है।
III
हमें अधीर नहीं होना चाहिए और तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
रुद्रवास और तपोवन की अवस्था से आनंदकानन-गौरपीठम और अविमुक्त क्षेत्र तक पहुँचने में कई शताब्दियाँ लगी होंगी। और फिर, उस अवस्था से वाराणसी के वास्तविक रूप में विकसित होने में भी कुछ और शताब्दियाँ बीती होंगी। वहाँ से इस्लामी आक्रमणों (1194 ईस्वी) के युग तक पहुँचना वैसा ही है जैसे इलियड, हित्तियों, सासानियों और सिकंदर के पूरे कालखंड को पार करना। बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, न ही ईसा मसीह प्रकट हुए थे। वाराणसी वास्तव में प्राचीन है, लेकिन जर्जर नहीं; यह पुरातन है, लेकिन अतीत के बोझ से दबी नहीं।
हम जिस वाराणसी के इतिहास की खोज कर रहे हैं, वह तथाकथित वैदिक काल से भी पहले शुरू होता है, क्योंकि वैदिकों का टकराव पहले से ही पहाड़ियों पर स्थापित एक अन्य संस्कृति से हुआ था।
आर्य प्रवासियों और पहाड़ियों में रहने वाले यक्षों और नागों के बीच प्रारंभिक संघर्ष, जैनियों और बौद्धों के बीच संघर्ष, और फिर बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच हुए संघर्षों ने महाश्मशान रुद्रवास की संरचना को बड़े पैमाने पर बदल दिया। इन तीव्र टकरावों की अनिवार्यता ने शिव-पशुपति को ब्राह्मणीय देवता के रूप में स्थापित किया, शक्ति को उनकी शक्ति-स्वरूपा बनाया, गणपति को उनका रक्षक, भैरव को सेनापति और सूर्य तथा नारायण को शांति स्थापना के साक्षी के रूप में स्वीकार किया गया।
आनंदकानन का हिंदू गढ़ हमेशा वैदिक अध्ययन का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा। हमें ज्ञात है कि दशाश्वमेध पर ब्रह्मवास और एक ब्रह्म सरोवर स्थित था। ह्वेनसांग ने भी वाराणसी में ब्राह्मणों और बौद्धों द्वारा संचालित विद्यालयों और महाविद्यालयों के अस्तित्व का उल्लेख किया है।
बुद्ध स्वाभाविक रूप से इस आध्यात्मिक केंद्र की ओर आकर्षित हुए, जैसे लोहा चुंबक की ओर खिंचता है। उन्होंने महसूस किया कि यदि उन्हें वैदिक सामाजिक संरचना को बदलना था और प्रकृति, जीवन और उसके परे के विषय में वैदिक व्याख्याओं को प्रतिस्थापित करना था, तो उन्हें वाराणसी के विद्वानों को प्रभावित करना आवश्यक था। वाराणसी हिंदू हृदय की आध्यात्मिक विजय की पूर्वपीठिका थी। आर्य मॉडल को केवल तभी प्रवेश मिल सकता था जब द्रविड़-प्रोलितारियट ने इसे सहज रूप से स्वीकार किया।
लेकिन जातकों के अनुसार, बुद्ध किसी विद्वान या कुलीन समाज के पास नहीं, बल्कि भीड़-भाड़ वाली व्यापारिक वाराणसी में आए। वे आदि शंकराचार्य की तरह तर्क-वितर्क करने नहीं आए थे, बल्कि जनता का हृदय जीतने आए थे।
इस बीच, वृक्षों से आच्छादित इस शांत स्थान का चरित्र बड़े पैमाने पर बदल गया था। हैहय और प्रतर्दन वंशों (जो संभवतः ययाति वंश के वंशज थे) के बार-बार होने वाले युद्धों ने वाराणसी के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित किया। इन युद्धों की गूँज वेदों, पुराणों और महाकाव्यों के पृष्ठों में दर्ज है। इसलिए, बुद्ध के लिए तपस्वी ब्राह्मण नहीं, बल्कि क्षत्रिय, वैश्य और उपेक्षित वर्ग अधिक महत्वपूर्ण थे। उन्होंने नगरों और उद्यानों में इन्हीं वर्गों को संबोधित किया।
इन संघर्षों को 'व्यवधान' कहा गया, जो यक्षों, गंधर्वों या सरल शब्दों में गणों से संबंधित थे। गणों को आमतौर पर पूर्व-आर्य श्रमिक वर्ग की विद्रोही शक्ति के रूप में देखा जाता था, जो सैन्य रूप से आक्रामक आर्यों के खिलाफ खड़े थे। इसे मौलिक तंत्र और वैदिक ब्राह्मणवाद के बीच टकराव के रूप में देखा जा सकता है।
हम पहले ही देख चुके हैं कि वाराणसी चारों ओर से गण-पूजास्थलों और बीर, भैरव तथा देव मंदिरों से घिरी हुई थी।
ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद, गणेश अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रखते हैं। उन्हें 'गणनायक' या 'सेनानायक' के रूप में सम्मानित किया जाता है। पौराणिक कथाएँ इस बात को प्रमाणित करने के लिए गढ़ी गईं कि गणेश को शिव और शक्ति के समान, या उनसे भी श्रेष्ठ रूप में स्वीकार किया जाए, ताकि वे वैदिक देवताओं की श्रेणी में समाहित किए जा सकें।
यह एक सिद्धांत हो सकता है, लेकिन अन्य सभी सिद्धांतों की तरह यह भी कुछ विशिष्ट ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। आज भी वाराणसी के चारों ओर कई स्मारक गणों और उनके निवास स्थलों की याद दिलाते हैं।
बीर, भैरव, सूर्य और गणदेवताओं (गणपति, गणनायक) के मंदिर आज भी जनता में अत्यधिक लोकप्रिय हैं, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो आर्य वर्गीकरण में 'उच्च' माने जाने वाले वर्गों से बाहर माने जाते हैं। ये मंदिर शिव के अनुयायियों द्वारा आक्रमणकारी आर्यों के विरुद्ध किए गए संघर्षों की स्मृति में बने हुए हैं।
इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैदिक विजेताओं को, अविमुक्त क्षेत्र (वह घाटी जहाँ से शिव या उनके गण अनुयायियों को निष्कासित नहीं किया जा सकता था) में स्थापित होने से पहले, स्थानीय देवताओं को स्वीकार करने की बुद्धिमानी अपनानी पड़ी।
इन उग्र योद्धाओं का सहयोग प्राप्त करना नवागंतुकों के लिए शांति से रहने के लिए आवश्यक था। उन्हें तंत्र-शिव और उनके अनुयायियों को स्वीकार करना पड़ा। विश्वनाथ वाराणसी के भैरव रूप में बने रहे, और विशालाक्षी (विशाल) उनकी शक्ति स्वरूपा बनी रहीं। इसे स्वीकार करने के बाद, नवागंतुकों ने आनंदकानन के सुखद वातावरण में अपने लिए एक शांतिपूर्ण स्थान पाया।
परिवर्तित होता नगर
IV
भैरव और भैरवी की जोड़ी एक विशेष संदेश देती है। हमें इस संदेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
पुराणों में विश्वनाथ को वाराणसी में सर्वोच्च स्थान नहीं दिया गया था। यह सम्मान पाँच अन्य महत्वपूर्ण लिंगों को प्राप्त था—अविमुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर, कृतिवासेश्वर, महाकालेश्वर और मध्येश्वर (महान पंचलिंग)।
जैसा कि हमें ज्ञात है, ये सभी लिंग वरुणा घाटी और मत्स्योदरी-मंदाकिनी परिसर के आसपास स्थित थे, अर्थात ज्ञानवापी ढलान के शीर्ष पर स्थित आदि-विश्वनाथ पर्वत से दूर।
ये पाँच लिंग वास्तव में वाराणसी के प्रधान लिंग थे। काशी खंड (क. ख.) विश्वनाथ को समान दर्जा नहीं देता। विश्वनाथ और अन्नपूर्णा को गौण देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है। (यह भी तंत्र पर वैदिक या आर्य उपेक्षा का एक और संकेत है।)
क्यों?
इसका उत्तर पाने के लिए हमें उस समय की प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों की पड़ताल करनी होगी, जो वाराणसी के समकालीन भक्तों को निर्देशित कर रही थीं। चूँकि आज महान पंचलिंग केवल नाममात्र के रूप में जाने जाते हैं, और उनके महान मंदिर धूल में समा चुके हैं, इसलिए वाराणसी में विश्वनाथ का महत्त्व पूर्ण रूप से उजागर हुआ है। पहले ऐसा नहीं था।
लेकिन वास्तव में, विश्वनाथ की भूमिका महान पंचलिंगों की भूमिका से बिल्कुल भिन्न थी। क. ख. और काशी महात्म्य (क. म्.) दोनों बताते हैं कि महान पंचलिंगों के मंदिर विभिन्न ऋषियों की प्रेरणा से स्थापित किए गए थे। प्रत्येक लिंग की स्थापना और प्रतिष्ठा से जुड़ी एक कथा है। लेकिन विश्वनाथ की कहानी अद्वितीय है। इसे किसी ने स्थापित या प्रतिष्ठित नहीं किया। इसे स्वयंभू (स्वतः प्रकट) कहा जाता है। (आधुनिक विश्वनाथ मंदिर स्वयंभू नहीं है।)
विश्वनाथ 'नाथ' हैं, और यह इस देवता के अघोरी तंत्र-शैव संप्रदाय में महत्त्व को दर्शाता है। इस प्रकार, यह वैदिक ऋषियों से पूर्णतः भिन्न मार्ग पर चला।
विश्वनाथ और विशालाक्षी (या विशाल) एक अत्यंत तांत्रिक जोड़ी के रूप में युगों से प्रतिष्ठित रहे हैं। ऐसे लिंगों को अनादि या स्वयंभू (पूर्व-आर्य?) लिंगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये वे लिंग हैं, जो बिना किसी प्रतिष्ठा के स्वयं प्रकट हुए, जबकि अन्य लिंगों की प्रतिष्ठा वैदिक ऋषियों ने की थी। स्वयंभू लिंग को प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती।
यह भी स्पष्ट करता है कि महान पंचलिंगों के मंदिर अत्यधिक समृद्ध थे और उनमें एकत्रित संपत्ति आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। इसके विपरीत, तांत्रिक विश्वनाथ मंदिर, जो एक भैरव मंदिर था, अकेले पहाड़ी के ऊपर स्थित था और संवेदनशील आर्य ऋषियों द्वारा उपेक्षित था। यह पहले हमलों से बचा रहा।
आज भी, परंपराओं के अनुसार, कठोर वैदिक ब्राह्मण अन्नकूट उत्सव के दौरान विश्वनाथ मंदिर के पके हुए प्रसाद को ग्रहण करने से हिचकिचाते हैं, जबकि अन्नपूर्णा का प्रसाद सहर्ष स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जब दिवाली के अवसर पर अन्नपूर्णा वार्षिक अन्नकूट उत्सव मनाती हैं, तब विशालाक्षी को लगभग अनदेखा कर दिया जाता है।
वाराणसी में तंत्र प्रवाह को प्रभावी रूप से पुराण प्रवाह द्वारा दबा दिया गया है। क. ख., क. म्., अग्नि पुराण, तीर्थ कल्पतरु और विविध तीर्थकल्प जैसी पुस्तकों ने स्थानीय मानसिकता को प्रभावित किया।
केवल तब, जब महान पंचलिंगों के मंदिर बार-बार नष्ट किए गए, यह संपूर्ण क्षेत्र अंधकार में चला गया और तब वाराणसी के लोगों ने बड़े धूमधाम से विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। अंततः यह भी एक लक्ष्य बन गया। लेकिन तब लोगों ने अपने प्रयास इस मंदिर को पुनः खड़ा करने में केंद्रित किए, क्योंकि अन्य मंदिर न केवल ध्वस्त कर दिए गए थे, बल्कि उनके स्थान पर इस्लामी संरचनाएँ भी बनाई गई थीं। उन मंदिरों के पुनर्निर्माण की कल्पना भी नहीं की गई।
इतिहासकार वाराणसी के मंदिरों की इस अस्थिर स्थिति से एक संदेश निकालते हैं। वे वाराणसी में तंत्र प्रवाह की प्रधानता को स्वीकार करते हैं और यह भी देखते हैं कि वैदिक प्रवाह ने बाद के निर्माणों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन जब इन संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया, तो उन्हें वापस उसी मूल तंत्र प्रवाह की ओर लौटना पड़ा, जिसे वे गौण मानते थे।
कोई इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत न भी हो, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि ध्वस्त किए गए पुराणिक मंदिर कभी पुनः नहीं उठे। वहीं, महान भैरव मंदिर, विश्वनाथ, बार-बार अत्यधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ पुनर्निर्मित किया गया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोगों के सामूहिक भक्ति-प्रवाह को रोका नहीं जा सका।
वाराणसी के प्राचीन क्षेत्र और इसके पाँच प्रमुख मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम एक अत्यधिक कठिन आर्थिक प्रयास होता, जिसे पूरा करना उस समय असंभव था, जब यह खतरा बना हुआ था कि भविष्य में फिर से कट्टरपंथी हमलों से इसे नष्ट किया जा सकता है। इतिहास ने यह दिखाया कि यह सावधानी व्यर्थ नहीं थी।
वास्तव में, नगर के संतुलन को झटका तब लगा जब वरुणा के तट और उसके मंदिर परिसर को मंदाकिनी झील के साथ नष्ट कर दिया गया। लोग किसी ठोस आश्रय की खोज में थे और उन्होंने स्वाभाविक रूप से दक्षिण और पश्चिम के वन क्षेत्रों में शरण ली। इस ऐतिहासिक संयोग के परिणामस्वरूप, मंदाकिनी ढलान के किनारे पहाड़ी पर स्थित मंदिर को अधिक महत्व मिलने लगा।
यह वही पहला मंदिर था, जो चौक पहाड़ी चढ़ने के बाद आता था, और यह मंदाकिनी तालाब से दूर स्थित था।
IV
भैरव और भैरवी की जोड़ी एक विशेष संदेश देती है। हमें इस संदेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
पुराणों में विश्वनाथ को वाराणसी में सर्वोच्च स्थान नहीं दिया गया था। यह सम्मान पाँच अन्य महत्वपूर्ण लिंगों को प्राप्त था—अविमुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर, कृतिवासेश्वर, महाकालेश्वर और मध्येश्वर (महान पंचलिंग)।
जैसा कि हमें ज्ञात है, ये सभी लिंग वरुणा घाटी और मत्स्योदरी-मंदाकिनी परिसर के आसपास स्थित थे, अर्थात ज्ञानवापी ढलान के शीर्ष पर स्थित आदि-विश्वनाथ पर्वत से दूर।
ये पाँच लिंग वास्तव में वाराणसी के प्रधान लिंग थे। काशी खंड (क. ख.) विश्वनाथ को समान दर्जा नहीं देता। विश्वनाथ और अन्नपूर्णा को गौण देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है। (यह भी तंत्र पर वैदिक या आर्य उपेक्षा का एक और संकेत है।)
क्यों?
इसका उत्तर पाने के लिए हमें उस समय की प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों की पड़ताल करनी होगी, जो वाराणसी के समकालीन भक्तों को निर्देशित कर रही थीं। चूँकि आज महान पंचलिंग केवल नाममात्र के रूप में जाने जाते हैं, और उनके महान मंदिर धूल में समा चुके हैं, इसलिए वाराणसी में विश्वनाथ का महत्त्व पूर्ण रूप से उजागर हुआ है। पहले ऐसा नहीं था।
लेकिन वास्तव में, विश्वनाथ की भूमिका महान पंचलिंगों की भूमिका से बिल्कुल भिन्न थी। क. ख. और काशी महात्म्य (क. म्.) दोनों बताते हैं कि महान पंचलिंगों के मंदिर विभिन्न ऋषियों की प्रेरणा से स्थापित किए गए थे। प्रत्येक लिंग की स्थापना और प्रतिष्ठा से जुड़ी एक कथा है। लेकिन विश्वनाथ की कहानी अद्वितीय है। इसे किसी ने स्थापित या प्रतिष्ठित नहीं किया। इसे स्वयंभू (स्वतः प्रकट) कहा जाता है। (आधुनिक विश्वनाथ मंदिर स्वयंभू नहीं है।)
विश्वनाथ 'नाथ' हैं, और यह इस देवता के अघोरी तंत्र-शैव संप्रदाय में महत्त्व को दर्शाता है। इस प्रकार, यह वैदिक ऋषियों से पूर्णतः भिन्न मार्ग पर चला।
विश्वनाथ और विशालाक्षी (या विशाल) एक अत्यंत तांत्रिक जोड़ी के रूप में युगों से प्रतिष्ठित रहे हैं। ऐसे लिंगों को अनादि या स्वयंभू (पूर्व-आर्य?) लिंगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये वे लिंग हैं, जो बिना किसी प्रतिष्ठा के स्वयं प्रकट हुए, जबकि अन्य लिंगों की प्रतिष्ठा वैदिक ऋषियों ने की थी। स्वयंभू लिंग को प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती।
यह भी स्पष्ट करता है कि महान पंचलिंगों के मंदिर अत्यधिक समृद्ध थे और उनमें एकत्रित संपत्ति आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। इसके विपरीत, तांत्रिक विश्वनाथ मंदिर, जो एक भैरव मंदिर था, अकेले पहाड़ी के ऊपर स्थित था और संवेदनशील आर्य ऋषियों द्वारा उपेक्षित था। यह पहले हमलों से बचा रहा।
आज भी, परंपराओं के अनुसार, कठोर वैदिक ब्राह्मण अन्नकूट उत्सव के दौरान विश्वनाथ मंदिर के पके हुए प्रसाद को ग्रहण करने से हिचकिचाते हैं, जबकि अन्नपूर्णा का प्रसाद सहर्ष स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जब दिवाली के अवसर पर अन्नपूर्णा वार्षिक अन्नकूट उत्सव मनाती हैं, तब विशालाक्षी को लगभग अनदेखा कर दिया जाता है।
वाराणसी में तंत्र प्रवाह को प्रभावी रूप से पुराण प्रवाह द्वारा दबा दिया गया है। क. ख., क. म्., अग्नि पुराण, तीर्थ कल्पतरु और विविध तीर्थकल्प जैसी पुस्तकों ने स्थानीय मानसिकता को प्रभावित किया।
केवल तब, जब महान पंचलिंगों के मंदिर बार-बार नष्ट किए गए, यह संपूर्ण क्षेत्र अंधकार में चला गया और तब वाराणसी के लोगों ने बड़े धूमधाम से विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। अंततः यह भी एक लक्ष्य बन गया। लेकिन तब लोगों ने अपने प्रयास इस मंदिर को पुनः खड़ा करने में केंद्रित किए, क्योंकि अन्य मंदिर न केवल ध्वस्त कर दिए गए थे, बल्कि उनके स्थान पर इस्लामी संरचनाएँ भी बनाई गई थीं। उन मंदिरों के पुनर्निर्माण की कल्पना भी नहीं की गई।
इतिहासकार वाराणसी के मंदिरों की इस अस्थिर स्थिति से एक संदेश निकालते हैं। वे वाराणसी में तंत्र प्रवाह की प्रधानता को स्वीकार करते हैं और यह भी देखते हैं कि वैदिक प्रवाह ने बाद के निर्माणों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन जब इन संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया, तो उन्हें वापस उसी मूल तंत्र प्रवाह की ओर लौटना पड़ा, जिसे वे गौण मानते थे।
कोई इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत न भी हो, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि ध्वस्त किए गए पुराणिक मंदिर कभी पुनः नहीं उठे। वहीं, महान भैरव मंदिर, विश्वनाथ, बार-बार अत्यधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ पुनर्निर्मित किया गया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोगों के सामूहिक भक्ति-प्रवाह को रोका नहीं जा सका।
वाराणसी के प्राचीन क्षेत्र और इसके पाँच प्रमुख मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम एक अत्यधिक कठिन आर्थिक प्रयास होता, जिसे पूरा करना उस समय असंभव था, जब यह खतरा बना हुआ था कि भविष्य में फिर से कट्टरपंथी हमलों से इसे नष्ट किया जा सकता है। इतिहास ने यह दिखाया कि यह सावधानी व्यर्थ नहीं थी।
वास्तव में, नगर के संतुलन को झटका तब लगा जब वरुणा के तट और उसके मंदिर परिसर को मंदाकिनी झील के साथ नष्ट कर दिया गया। लोग किसी ठोस आश्रय की खोज में थे और उन्होंने स्वाभाविक रूप से दक्षिण और पश्चिम के वन क्षेत्रों में शरण ली। इस ऐतिहासिक संयोग के परिणामस्वरूप, मंदाकिनी ढलान के किनारे पहाड़ी पर स्थित मंदिर को अधिक महत्व मिलने लगा।
यह वही पहला मंदिर था, जो चौक पहाड़ी चढ़ने के बाद आता था, और यह मंदाकिनी तालाब से दूर स्थित था।
V
इस संदर्भ में, जैन और बौद्ध धर्म की सारनाथ परंपरा और उन पवित्र स्थलों में तांत्रिक साधनाओं की प्रगति को याद करना सहायक होगा। अतीश श्रीज्ञान, पद्मसंभव और बाद में नागार्जुन के आगमन के बाद बौद्ध साधनाओं में व्यापक परिवर्तन आया। विशेष रूप से महायान परंपरा ने आम जनता को प्रभावित किया। अश्वघोष, वसुमित्र और अभिनवगुप्त की रचनाओं ने जनमानस को अभिभूत कर दिया। सारनाथ तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र बन गया। गाहड़वाल वंश की रानी कुमारदेवी की इस परंपरा में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।
इन लोकप्रिय तांत्रिक प्रथाओं के प्रभाव में, विश्वनाथ और भैरव मंदिरों ने, गणपति मंदिरों के साथ, वाराणसी (या वाराणवती) के ध्वस्त मंदिरों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली।
अब, हमें दो महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करनी होगी, जो इस संदर्भ में बार-बार प्रयुक्त होते हैं—'पीठ' और 'क्षेत्र'। वाराणसी को 'क्षेत्र' कहा जाता है, और इसे 'गौरीपीठ' भी कहा जाता है। यदि हम इन शब्दों के निहितार्थ को समझें और यह जानने का प्रयास करें कि वाराणसी को 'क्षेत्र' और 'पीठ' दोनों क्यों कहा जाता है, तो हम यह भी समझ पाएँगे कि वाराणसी को युगों से रुद्र केंद्र, तंत्र केंद्र और वाम तांत्रिक साधना केंद्र के रूप में क्यों सम्मानित किया गया है।
यह समझने के बाद, हमें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि अन्य सभी नगरों में से केवल वाराणसी को ही 'काशी विश्वनाथ का क्षेत्र' क्यों कहा जाता है।
'क्षेत्र' और 'पीठ' दोनों में तांत्रिक अर्थ निहित हैं। हालाँकि, यह 'धाम' के मामले में नहीं है, जो तीर्थ केंद्रों से जोड़ा जाने वाला एक अन्य प्रत्यय है। चूँकि 'क्षेत्र' और 'पीठ' का संबंध तंत्र से है, जबकि 'धाम' मुख्य रूप से वैष्णव भावधारा को व्यक्त करता है। इस प्रकार, 'धाम' मुख्य रूप से वैष्णव तीर्थ होते हैं, जबकि 'पीठ' और 'क्षेत्र' आमतौर पर तांत्रिक स्थल होते हैं।
'क्षेत्र' तंत्र में हमेशा एक विशेष महत्व रखता है। संस्कृत में 'क्षेत्र' का अर्थ संपूर्ण शरीर या स्त्री के उस अंग से भी है जहाँ से सृजन उत्पन्न होता है। शब्दकोश भी इस अर्थ को मान्यता देते हैं और यह भी बताते हैं कि त्रिकोणीय आकृति को भी 'क्षेत्र' कहा जाता है। तंत्र में 'क्षेत्र' और 'लांगल' (हल) के प्रतीकात्मक अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं।
इसलिए तीर्थस्थलों में वे स्थान, जो मुख्य रूप से तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्हें 'क्षेत्र' कहा जाता है।
'पीठ' शब्द का तंत्र में प्रयोग शिव और सती की कथा से जुड़ा हुआ है, जब विष्णु को शोकाकुल शिव द्वारा ढोए जा रहे सती के शरीर को खंड-खंड करना पड़ा, ताकि वे शोक के भार से मुक्त हो सकें। देवी के शरीर के अंग जहाँ-जहाँ गिरे, वे स्थान 'पीठ' के रूप में पवित्र हो गए।
इस प्रकार, पीठ सामान्यतः गैर-वैदिक परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। पीठों पर बड़े मंदिरों का निर्माण बहुत दुर्लभ होता है। 'पीठ' का अर्थ 'आसन' होता है, न कि मंदिर। सामान्यतः ये पूजा स्थल होते हैं, जिनके आसपास अधिक भव्यता नहीं होती।
यह इस कारण है कि तंत्र स्थलों की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कहीं दूर, निर्जन स्थान में कोई ऐसा तांत्रिक स्थल अचानक मिल जाए, जिसे एकमात्र साधक पूजित करता हो। (जैसे, शिमला के पास तारादेवी मंदिर, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में तिरोल गाँव की काली, विंध्याचल में अष्टभुजा, बाँकुड़ा में योगिनी, काशी में तारा, एलोरा में गरसंसा और रांची में राजरप्पा की छिन्नमस्ता।)
यहाँ तक कि विश्वालक्षी (विशालाक्षी) का वाराणसीपीठ बिना अधिक प्रचार के संरक्षित रह गया और हमलावरों के विनाश से बच गया। यही स्थिति मीर घाट, वाराणसी में स्थित अत्यंत अल्पज्ञात वाराही मंदिर की भी रही।
मंदिरों की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। मंदिर संस्कृति कभी भी भारतीय उपमहाद्वीप की मूल संस्कृति नहीं रही। इसका ऐतिहासिक प्रारंभ विदेशी संस्कृतियों के आगमन के साथ हुआ, जो व्यापारियों, यात्रियों, विशेष रूप से यूनानियों और शकाओं द्वारा लाई गई थी।
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण पश्चिमी एशिया (ईरान, अरब और खाड़ी क्षेत्र सहित) मुख्य रूप से एक विस्तृत और प्रभावशाली 'मंदिर संस्कृति' के अधीन था। मिस्र, सीरिया, इराक, यूनान, साइप्रस और फारस पुजारियों के समुदाय के नियंत्रण में थे। भारत का इन देशों से व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से घनिष्ठ संबंध था। इस प्रकार, यह संस्कृति भारत में स्वतः ही प्रवेश कर गई।
यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि हमारे पुराणों में वाराणसी को विशेष रूप से चार पवित्रतम तीर्थों के लिए जाना जाता है—मणिकर्णिका ह्रद (झील), चक्रतीर्थ, ज्ञानवापी और पंचगंगा।
विशेष रूप से ये सभी स्नान स्थल थे, जिनके आसपास कोई मंदिर या मानव बस्तियाँ नहीं थीं। इन तीर्थों के चारों ओर केवल वृक्ष, उद्यान, पूजास्थल और आश्रम थे।
और निश्चित रूप से, महान और पवित्र गंगा यहाँ अनादि काल से शांतिपूर्वक प्रवाहित होती रही है।
मणिकर्णिका के चारों ओर का क्षेत्र अन्य महत्वपूर्ण तत्वों से भी समृद्ध था।
VI
हमने देखा कि प्राचीन वाराणवती नगर वरुणा नदी के दोनों किनारों पर स्थित था, जहाँ अनेक मंदिरों की कतारें थीं। लेकिन जब कोई मानव बस्ती स्थायी रूप से स्थापित होती है, तो उसे अन्य सुविधाओं के साथ-साथ मृतकों के अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था करनी पड़ती है।
मृतकों का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाता था? हमने देखा है कि अठारहवीं शताब्दी में ही मणिकर्णिका-ब्रह्मनाल को श्मशान स्थल के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। इसका अर्थ यह हुआ कि अतीत में अन्य व्यवस्थाएँ अवश्य रही होंगी। यह व्यवस्थाएँ दूर स्थित हरिश्चंद्र घाट (चेत सिंह किले के पास) या खिड़की घाट नहीं हो सकती थीं। फिर, कौन-से घाट अंतिम संस्कार के लिए उपयोग किए जाते थे?
हम जानते हैं कि वारुणा और गंगा नदी के संगम पर एक श्मशान स्थल स्थित था। कुछ लोग अब भी इसे श्मशान स्थल के रूप में उपयोग करते हैं। इसके निकट ही दत्तात्रेय का एक छोटा सा मंदिर है।
आमतौर पर, श्मशान घाटों को न तो जीवित बस्तियों के बहुत निकट बनाया जाता था, न ही अत्यधिक दूर। यदि मुख्य नगर मत्स्योदरी-मंदाकिनी परिसर और वरुणा के तट पर विकसित हुआ था, और त्रिलोचन तथा पंचगंगा तक फैला था, तो श्मशान घाट बहुत दूर नहीं हो सकते थे।
वे वास्तव में अधिक दूर नहीं थे।
जब गाहड़वाल वंश के किले के निर्माण के कारण नगर अधिक घनीभूत हो गया, तो संगम के निकट स्थित श्मशान को अपेक्षाकृत निर्जन दक्षिणी भाग में स्थानांतरित कर दिया गया। संकट घाट के पास एक 'यम घाट' स्थित है। 'यम' नामक इस स्थल की उपस्थिति श्मशान स्थल होने का संकेत देती है, और यमधर्मेश्वर मंदिर इस अनुमान की पुष्टि करता है।
कुछ समय बाद, नगर का विस्तार और दक्षिण की ओर बढ़ा, और इसके साथ ही श्मशान स्थल भी स्थानांतरित कर दिया गया।
आज, हम हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर को इस नए स्थल के निकट पाते हैं और यह अनुमान लगा सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की कथा ने उन्हें इसी स्थान पर (न कि केदार घाट के पास) अपने स्वामी के साथ काम करने के लिए लाया था। आधुनिक हरिश्चंद्र घाट वास्तव में एक प्रतिस्थापन है, जो तब अस्तित्व में आया जब उत्तरी श्मशान घाट को बंद कर दिया गया। यदि आगे पुष्टि की आवश्यकता हो, तो यह कहा जा सकता है कि इसी स्थान पर आज भी यम द्वितीया या भाई दूज का अनुष्ठान और स्नान किया जाता है। यम मृत्यु के देवता हैं।
चूँकि वारुणा संगम के पास स्थित मूल दत्तात्रेय मंदिर बंद कर दिया गया था, इसलिए इस नए स्थान के पास एक नया दत्तात्रेय मंदिर स्थापित किया गया, जहाँ अब भी एक श्मशान विनायक मंदिर स्थित है।
वाराणसी के गंगा तट तंत्र साधकों के लिए सदा से ही अनुष्ठान स्थल रहे हैं, और 'महाश्मशान' नाम, जिससे वाराणस्या को पहले जाना जाता था, इसके प्राचीन स्वरूप का पूर्ण वर्णन करता है।
इसके अलावा, परंपराओं के अनुसार, मीर घाट और मानसिंह घाट (मनमंदिर घाट) को भी कभी श्मशान स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था। ये प्रयाग घाट और दशाश्वमेध घाट के निकट स्थित थे।
गंगा के किनारे श्मशान स्थल के स्थानांतरण का अध्ययन हमें तीन प्रमुख निष्कर्ष देता है:
1. पूर्व-वैदिक काल में गंगा के तटों का श्मशान के रूप में उपयोग किया जाता था, जिससे वाराणसी को 'महाश्मशान' कहा जाता था।
2. वाराणसी की पहाड़ी श्रृंखला मुख्य रूप से तांत्रिक परंपरा से संबंधित थी, और इस क्षेत्र के लिए 'गौरीपीठ' नाम अत्यंत उपयुक्त था।
3. जब नगर का विस्तार हुआ और आनंदकानन को समाहित कर लिया गया, तब नगर का विकास धीरे-धीरे वरुणा तट से असि तट की ओर बढ़ा।
तांत्रिक प्रभाव की प्रधानता के कारण, और क्योंकि वाराणवती के प्रमुख भैरव स्वयं शिव विश्वेश्वर थे, उनकी शक्ति विशाल (विशालाक्षी) थी, तथा इस पवित्र स्थान के संरक्षक भैरवों और गणदेवों के समूह थे, जिनमें काल भैरव प्रमुख थे, इसलिए विश्वेश्वर लिंग को सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली। कृतिवास, ओंकार, महाकाल, अविमुक्त और मध्येश्वर का समूह, जो वैदिक काल में बाद में जोड़े गए, कभी भी तंत्र-स्वरूप विश्वेश्वर के समान लोक श्रद्धा प्राप्त नहीं कर सके।
महान पंचलिंगों और बिंदुमाधव के मंदिरों को ध्वस्त किए जाने के बाद, वे कभी पुनर्निर्मित नहीं किए गए। वास्तव में, उनमें से अधिकांश भुला दिए गए। इसके विपरीत, विश्वेश्वर मंदिर बार-बार पुनर्निर्मित किया गया, और 'विश्वासियों' के विरोध के बावजूद, विश्वनाथ हिंदू श्रद्धा का केंद्र बने रहे। आज काशी ही विश्वनाथ है, और विश्वनाथ ही काशी।
'तीर्थ विवेचन खंड' (लक्ष्मिधर) वाराणसी में शैव-तंत्र को लोकप्रिय धर्म के रूप में स्वीकार करता है। तंत्र की लोकप्रियता निर्विवाद थी। मोतीचंद्र ने 'मत्स्य पुराण' को उद्धृत करते हुए बताया कि ब्राह्मणीय युग में अविमुक्तेश्वर, न कि विश्वनाथ, वाराणसी का प्रमुख देवता था। 'लिंग पुराण' गाहड़वाल युग से लगभग डेढ़ शताब्दी पहले लिखा गया था। लक्ष्मिधर के 'कृत्य कल्पतरु' में लिंग पुराण को उद्धृत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि विश्वनाथ का स्थान सदा ज्ञानवापी सरोवर के पास रहा। यद्यपि कुछ समय के लिए अविमुक्त वाराणसी का प्रधान मंदिर बन गया था, फिर भी विश्वनाथ वाराणसी में शैव तंत्र के केंद्र बने रहे, जिसने राजा गोविंदचंद्र की पत्नी कुमारदेवी को अत्यधिक आकर्षित किया।
इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रभाव (संभवतः राजसी, ब्राह्मणीय या दोनों) के कारण, वरुणा के तट पर निर्मित मंदिरों को कुछ समय के लिए अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।
लेकिन इस पक्षपात और परंपरागत महत्वपूर्ण देवताओं की उपेक्षा का कारण क्या था?
जब ह्वेनसांग ने पहली बार वरुणा के तट पर मंदिरों की श्रृंखला देखी, तब से लेकर अब तक वे सभी पूर्णतः नष्ट कर दिए गए। मत्स्योदरी तक उपेक्षित रही। बड़े बरकरीकुंड और उसके मंदिरों की पूरी बस्ती नष्ट कर दी गई। पुनर्निर्माण का कोई प्रयास नहीं किया गया, सिवाय कुछ छोटे-छोटे स्थानों को यहाँ-वहाँ समाहित करने के। अविमुक्तेश्वर, जिसे ब्राह्मणीय ग्रंथों में वाराणसी का प्रधान देवता माना गया था, आधुनिक विश्वनाथ मंदिर के भीतर एक कोने में स्थित है, एक गौण स्थान पर। यह आश्चर्यजनक है कि जब अकबर और जहानदार शाह ने पुनर्निर्माण की अनुमति दी, तब भी इन पाँच प्रमुख देवताओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया गया।
अंततः जब मराठों द्वारा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और ज्ञानवापी को पुनः निर्मित किया गया, तब भी किसी ने महान पंचलिंगों की पुनः स्थापना के बारे में नहीं सोचा। लेकिन कोई भी विश्वनाथ को उपेक्षित नहीं कर सका। वाराणसी में तंत्र परंपरा ब्राह्मणीय प्रभाव से अधिक सशक्त सिद्ध हुई।
परिवर्तित होता नगर
VII
गंगा युग से देव युग में परिवर्तन होने में कई शताब्दियाँ बीती होंगी, जब तक कि इतिहास में दस राजाओं के युद्ध, सुर-असुर संघर्ष, कुरुक्षेत्र, जरासंध और फिर कालचुरी, शक, पुलिंद और अंततः प्रतर्दन, दिवोदास, हैहय और गाहड़वाल वंश के उल्लेख नहीं मिलने लगे।
इसीलिए, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि गण-शिव और रुद्र-शिव के आनंदकानन का नाम बदलकर वाराणसी तब किया गया जब वरुणा नदी राजसी प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण हो गई, और असि नदी उनके आधिपत्य की सीमा निर्धारित करने के लिए चुनी गई। यह नाम उन उत्पीड़ित लेकिन मूल निवासियों द्वारा ग्रहण किया गया था जो महाश्मशान, गौरीपीठ और रुद्रवास के मूल निवासी थे।
परंतु यह नाम अधिक समय तक स्थिर नहीं रहा। यह जैन, बौद्ध और अन्य समुदायों के बीच हुए धार्मिक संघर्षों (अजातशत्रु, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) के दौरान फिर से परिवर्तनों से गुज़रा।
वाराणसी द्वारा 'काशी' को राज्य-नाम के रूप में अपनाने की घटना इसी काल में हुई होगी, और पुराणों एवं महाकाव्यों में इसके अंधाधुंध उल्लेख से यह भ्रम स्थापित हुआ। (वृज्जि अभिलेख देखें।) इस भ्रम का प्रमाण संत अगस्त्य के प्रश्न से भी मिलता है, जो काशीखंड में उल्लिखित है।
हैहय और कालचुरी के आक्रमणों की श्रृंखला ने गाहड़वाल राजाओं (दसवीं शताब्दी ईस्वी) को अपनी राजधानी दक्षिणी पहाड़ियों की ओर स्थानांतरित करने के लिए विवश किया। इस प्रकार, प्राचीन आनंदकानन की पहचान वाराणसी नाम से स्थापित हो गई, क्योंकि असि जलधारा भी इस चरण में सम्मिलित हो गई। वनाच्छादित क्षेत्र अब एक नगरीय नाम धारण कर चुका था। एक महानगरीय संस्कृति ने तपोवन संस्कृति को धीरे-धीरे निगल लिया।
इन सभी विनाशों के बाद, देव, गण, जैन और बौद्ध काल के बाद अफगान और मुग़ल आक्रमणों का सबसे क्रूर दौर आया। 'विश्वासियों' की एक नई मिलीटन्ट धारा ने मूर्तिपूजक 'काफिरों' को सुधारने के नाम पर पश्चिम से आक्रमण किया।
धार्मिक वाराणसी के प्राचीन अवशेष इस क्रूर दबाव के आगे बिखर गए।
VII
अब हम इन विनाशकारी परिवर्तनों की कल्पना वास्तविक टनों मलबे और सदियों से जमा हुई ध्वंसावशेषों के संदर्भ में करें।
हर आक्रमण के बाद, जब तक भय का खतरा बना रहा, किसी ने भी एक ईंट या पत्थर हटाने का साहस नहीं किया। पुनर्निर्माण की तो कोई कल्पना भी नहीं थी।
मलबे के ढेर बढ़ते गए, और गंदगी ने चारों ओर फैलकर परिवेश को दूषित कर दिया। पवित्र तालाब धीरे-धीरे अवरुद्ध हो गए। जहाँ नर्तकियाँ अपने देवताओं को समर्पित होकर नृत्य करती थीं, वहाँ अब भेड़िए, जंगली सूअर और गीदड़ घूमने लगे। झाड़-झंखाड़ और बाँस की झाड़ियाँ उन स्थलों को ढँकने लगीं जो कभी भक्तों के मिलन स्थल हुआ करते थे। बगीचे उजाड़ जंगलों में बदल गए। फव्वारे सूख गए। संगीत और नाटक के आयोजन स्थल अब साँपों, सूअरों, कुत्तों और गिद्धों के आश्रय स्थल बन गए।
खोए हुए मंदिर स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए, मलबे के पहाड़ों को हटाने की आवश्यकता थी। बिना इन्हें हटाए, कोई नया आरंभ संभव नहीं था।
यह सफाई अभियान एक विशाल परियोजना बन गया। इसके दायरे की विशालता ने सबसे साहसी लोगों को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी प्रयास जारी रहे। निर्धन और वंचित लोग अपने विफल देवताओं को पुनः स्थापित करने के लिए परिश्रम करते रहे। वे झुके हुए शरीरों से नए मंदिर उठाने में सहायता करते रहे। बार-बार भक्तों ने प्रयास किया, और बार-बार नए आक्रमणों ने पहले के सभी प्रयासों को धूल में मिला दिया।
लेकिन यह उल्लेखनीय है कि किसी ने भी छोटे रास्ते के मंदिरों या गरीब देवताओं को नहीं छुआ। प्राचीन देव और बीर मंदिर लगभग बिना किसी क्षति के बच गए। समृद्ध मंदिर ही विशेष रूप से 'विश्वासियों' के ग़ुस्से के लक्ष्य बने। जो लोग बाह्य मूर्तिपूजा को हटाने आए थे, वे अपनी आंतरिक लालसा, लोभ और हिंसा को नष्ट नहीं कर सके। ये देवताओं के लिए असली दानव थे।
इसलिए, हमारा कार्य अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। हमें खोई हुई आनंदकानन-वाराणसी का पुनर्निर्माण करना होगा, जैसा कि पुराणों (वायु, अग्नि, काशीखंड) में वर्णित है या जैसे यात्रियों—फा-हियान, ह्वेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता, टवर्नियर और अन्य ने रिपोर्ट किया।
वर्षों से पवित्र माने जाने वाले कई तालाब, झीलें और नदियाँ अब पहचान से परे नष्ट कर दी गईं। विनाशकारी ताकतों ने सदियों तक मलबे और कचरे को इन्हीं जल निकायों में डालना आसान समझा। जब तक इन ढेरों को समतल नहीं किया गया, तब तक भूमि पुनः प्राप्त करना असंभव था। सड़ते हुए तालाबों से उठने वाली दुर्गंध ने वातावरण को विषाक्त कर दिया।
वाराणसी को प्लेग, हैजा, चेचक और मलेरिया जैसी महामारियों का स्थायी खतरा बना रहा।
वाराणसी को पुनः जीवंत करने की इस नई उत्सुकता ने कभी यह विचार नहीं किया कि उनकी अकस्मात् की गई उत्सुकता मानव जीवन को जल स्रोतों जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से काट सकती है, या कि उनके इस विचारहीन कृत्य से महान सांस्कृतिक इतिहास के प्राकृतिक प्रमाण स्थायी रूप से मिट सकते हैं।
हमारी प्रवृत्ति प्राचीन धरोहरों के संरक्षण में अत्यंत उदासीन रही है। हम ऐतिहासिक स्मृतियों के संरक्षण को सांस्कृतिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखते। जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता के दर्शन से प्रभावित होकर, हम स्थायित्व और निरंतरता की परवाह नहीं करते।
आज भी, हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करने की अनुमति देते हैं।
1997 तक, वाराणसी के 50 से अधिक प्रमुख तालाबों में से एक भी शेष नहीं रहा। लक्ष्मीकुंड, सूरजकुंड, पिशाचमोचन, ईशरगंगा, बकरियाकुंड, कुरुक्षेत्र, खोजवातालाब, रेवतीकुंड और रेउरतालाब जैसे महान जल निकाय या तो मर चुके हैं या मरने की कगार पर हैं। इस उपेक्षा के लिए हम किसी विदेशी हस्तक्षेप को दोष नहीं दे सकते। हमारे अपने जीवन और सोचने के तरीकों ने यह आत्मघाती परिवर्तन किया है।
इस अंधी नगरीकरण की दौड़ ने सुंदर आनंदकानन तपोवन को स्थायी रूप से नष्ट कर दिया। इसकी प्राकृतिक शांति राजनीतिक मूर्खताओं और संपत्ति की लालसा के कारण वाष्पित हो गई।
और आज, जब विनाश की यह प्रक्रिया जारी है, तो हम दोष किसे दें—सिवाय अपने आप को?
VIII
भूगोलिक और पुरातात्विक प्रमाणों से यह स्थापित हो चुका है कि प्राचीन वाराणसी आधुनिक राजघाट क्षेत्र की ऊँचाइयों पर स्थित थी और यह अब भूले जा चुके, परंतु तब प्रसिद्ध मत्स्योदरी और मंदाकिनी झीलों के किनारे फैली हुई थी।
शिलालेखों से ज्ञात होता है कि गाहड़वाल वंश के राजाओं और उनकी रानियों ने वाराणसी पर शासन किया और वे "वरुणा संगम में स्नान करते थे तथा आदि-केशव की पूजा करते थे।"
झील के किनारों से सटे इस विस्तृत भू-भाग को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। पतंजलि (द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व) ने भी इस व्यापारिक केंद्र का उल्लेख किया है। हमने देखा कि समृद्ध बाज़ारों की उपस्थिति के कारण वाराणसी को 'जित्वारी' अर्थात 'लाभ का नगर' कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में भी यह बाज़ार सक्रिय था, और आज भी यह वाणिज्य का केंद्र बना हुआ है। फा-हियान, ह्वेनसांग और बाद के तुर्को-अरबी यात्रियों ने इन बाज़ारों की भीड़ और उत्पादों का विस्तृत वर्णन किया है। आज भी एक व्यापारिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति इन बाजारों की व्यस्तता को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।
आज भी वाराणसी का वाणिज्य मुख्य रूप से इन्हीं बाज़ारों में संचालित होता है। ये बाज़ार अब भी विश्वेश्वरगंज (विश्वेश्वर का बाज़ार), लक्ष्मीचबूतरा, कुंजरटोला और ठठेरी बाज़ार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस व्यस्त क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग अब भी 'पक्की मोहल्ला' (रूढ़िवादी समाज में) या 'ऊँची मोहल्ला' (ऊँचाई पर स्थित बस्ती) के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में, यही वाराणसी नगर का मूल केंद्र था। हेस्टिंग्स का चेत सिंह पर आक्रमण करने के लिए इस स्थान को चुनना रणनीतिक रूप से उचित था।
लगातार सैन्य उथल-पुथल के बावजूद आनंदकानन का हृदय अडिग बना रहा। काशी राज्य, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वनाच्छादित आनंदकानन के साथ सह-अस्तित्व में रहा, हालांकि उत्तर-पश्चिम में लगातार सैन्य आक्रमणों से भागे व्यापारिक और सांसारिक शरणार्थियों के अचानक प्रवाह ने इस प्राचीन वन क्षेत्र के मूल स्वरूप को काफी बदल दिया।
पहले लुटेरों की लालच, और फिर दूरस्थ व्यापारियों के कठोर व्यावसायिक स्वार्थ ने अंततः वाराणसी की शांति को समाप्त कर दिया। वास्तविक आनंदकानन मानव लोभ, धार्मिक कट्टरता और प्राचीन परंपराओं के प्रति उदासीनता से नष्ट हो गया।
विदेशियों द्वारा छोड़ा गया विनाश आज के नगर नियंताओं द्वारा बदले की भावना से पूरा किया जा रहा है।
इस परिवर्तनशील नाट्यक्रम में, ओंकारखंड और विश्वनाथखंड को सबसे अधिक क्षति पहुँची। काशीखंड में वर्णित नदियाँ, तालाब और झीलें, जो इस क्षेत्र का हिस्सा थीं, लगभग पूरी तरह से विलुप्त हो गईं। इस नुकसान ने गोदावरी धारा, अगस्त्यकुंड, भूतश्वर और प्रसिद्ध ज्ञानवापी जैसे जल स्रोतों को समाप्त कर दिया।
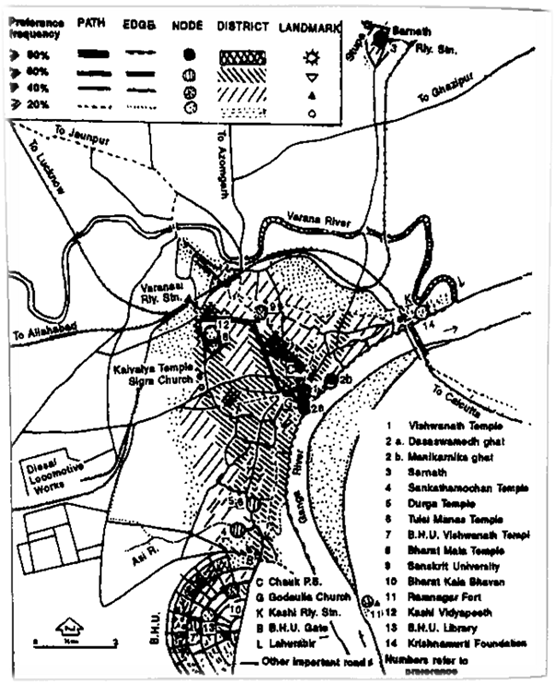
मानचित्र 11. वाराणसी: एक समग्र संज्ञानात्मक मानचित्र-रेखाचित्र
प्राकृतिक संपदा को धर्म या व्यापार के नाम पर नष्ट करना प्राकृतिक सुंदरता के प्रति घोर उदासीनता को दर्शाता है। यह संस्कृति के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराधों में से एक है।
इस्लामी आक्रमणकारी लूट में रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी प्राकृतिक पर्यावरण को विशेष रूप से क्षति नहीं पहुँचाई। वे जलस्रोतों और बाग़ों को लेकर सतर्क थे। जो भी प्राकृतिक सुंदरता उन्होंने छोड़ी थी, उसे ब्रिटिश प्रशासन ने 'नगर विकास' के नाम पर व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया।
वाराणसी के जलस्रोतों के विनाश ने इसकी आत्मा और ऊर्जा को अपूरणीय क्षति पहुँचाई। आनंदकानन अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। पहाड़ियाँ, वन, झीलें और नदियाँ अब केवल स्मृतियों में ही बची हैं। कौन आज मंदाकिनी झील को याद करता है?
हाँ, बारहवीं शताब्दी से लगातार हो रहे विनाश, (या इससे भी पहले जैन-बौद्ध प्रभाव से ब्राह्मणीय व्यवस्था को मिली चुनौती) ने प्राचीन वाराणसी की भव्यता को गंभीर क्षति पहुँचाई।
आज की वाराणसी में हमें काशीखंड या चीनी यात्रियों द्वारा वर्णित आकर्षक भौगोलिक विशेषताओं के कोई संकेत नहीं मिलते।
इन सभी ऐतिहासिक अभिलेखों में प्रभावशाली मंदिरों की एक श्रृंखला का उल्लेख है, जो भीड़भाड़ वाले बाज़ारों से घिरी हुई थीं। इन बाज़ारों में देश के विभिन्न भागों से दुर्लभ और महंगे वस्त्र एवं सामग्री लाई जाती थीं।
पर्यटकों और श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए प्रशिक्षित नर्तकियाँ, संगीत समारोह, कठपुतली प्रदर्शन, कुश्ती और नौका प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती थीं।
ये सब कहाँ चले गए? वह प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर 'मोक्ष-लक्ष्मी-विलास' कहाँ खो गया? आधुनिक विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर एक महान महाकाव्य की विकृत छाया मात्र प्रतीत होते हैं।
चूँकि ह्वेनसांग ने स्वयं इस मंदिर परिसर को देखा था, यह पाँचवीं शताब्दी से भी अधिक प्राचीन रहा होगा, यहाँ तक कि यह सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के उपदेश समाप्त होने से भी पहले का हो सकता है।
12.वह मरने से इनकार करती है
I
वाराणसी को पहला आघात ग्यारहवीं शताब्दी के अंत में तब सहना पड़ा जब महमूद गज़नी ने इस पर आक्रमण किया।
यह उस भयंकर घटना का वर्णन करने के लिए एक उपयुक्त विराम हो सकता है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्रहवीं शताब्दी ईसा पूर्व से बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक, लगभग 2000 वर्षों तक आनंदकानन ने अपनी स्वर्गीय शांति और दिव्य वैभव का आनंद लिया। चूँकि वाराणसी की प्राचीनता आर्यों के आगमन से भी पहले की मानी जाती है, यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि यह पौराणिक कानन, अर्थात आनंदवन, पहाड़ियों और वरुणा तट के आसपास एक शांतिपूर्ण परंपरा स्थापित कर चुका था, जो अभी पूर्णतः नगरीकृत नहीं हुआ था।
ऐसा प्रतीत होता है कि वाराणसी की धूल में कोई रहस्यमयी, चिरस्थायी जीवन-शक्ति समाहित है। जब पुरुषपुर, वराहमूल, तक्षशिला, धारा, अवंती, श्रावस्ती, कन्नौज, वैशाली, नालंदा, कौशांबी, अहिच्छत्र, यहाँ तक कि मृगदाव तक मिट गए, तब भी वाराणसी बनी रही।
वाराणसी गिरती है, धूल से उठती है, फिर गिरती है और फिर उठ खड़ी होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई रहस्यमयी और चिरस्थायी जीवन-शक्ति अंतर्निहित है। वाराणसी मरने से इनकार करती है। उसके शत्रु बार-बार उसके वयोवृद्ध सिर पर राख और आग बरसाते हैं, और वह फिर भी ध्वंस के ढेर से अपना घायल सिर उठाती है।
यह अप्रत्याशित त्रासदी 1194 ईस्वी में घटी। लेकिन वाराणसी की लोचपूर्ण जीवटता ने बार-बार आने वाले विनाश को नकार दिया और वह फिर से पुनर्जीवित हुई, जैसे मिस्र के 'अमर पिरामिड'।
II
हम थोड़ा पीछे चलते हैं और ऐला-पुरुरवा से प्रारंभ करते हैं, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान (आधुनिक प्रयाग के निकट झूंसी) में थी। 'चंद्रवंशी' शासकों ने काशी पर जयचंद के काल (1194 ईस्वी) तक शासन किया, जो घोरी-पृथ्वीराज संघर्ष में कुख्यात हुआ।
पुरुरवा से प्रारंभ करते हुए, आइए कुछ तीव्र गति से इतिहास का अवलोकन करें और पृष्ठभूमि को ठीक से स्थापित करें, ताकि हम अमर वाराणसी की अवधारणा को सही रूप में समझ सकें और उसके गौरव और अपमान के अध्यायों को एक चित्र की भाँति व्यवस्थित कर सकें।
पुरुरवा और मगध साम्राज्य के बीच 28 पीढ़ियों तक चंद्रवंशी राजाओं ने काशी पर शासन किया, जिसके बाद कोसल शासकों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। फिर मौर्य आए, उनके बाद शुंग, कण्व और कुषाण। कनिष्क, जो मूलतः विदेशी था, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसके सरल जीवन-दर्शन से मोहित हो गया। उसने स्वयं को भारतीय जीवनधारा के साथ एकाकार कर लिया और एक भारतीय सम्राट के रूप में शासन किया।
इसके बाद कुषाणों का शासन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। स्थानीय भरा-शिव समुदाय ने आनंदकानन वाराणसी का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और वाराणसी की पहाड़ियों पर पारंपरिक लिंग और भैरव पूजन पुनः स्थापित हो गया। शिव लिंग रूप में और शक्ति योनि या गौरीपीठ रूप में एक साथ पूजे जाने लगे, जो जीवन-स्रोत के रूप में उनके लिए ब्रह्मांडीय प्रतीक थे। यह द्वैत में अद्वैत उन्हें समस्त सृष्टि का मूल प्रतीत हुआ।
इसके बाद गुप्त वंश आया, उसके बाद थानेश्वर के शासक और फिर हर्षवर्धन। राजनीतिक रूप से, वाराणसी गुप्त सम्राटों के संरक्षण में आई, जो ब्राह्मणीय आस्था को मानने वाले थे। उनके द्वारा वाराणसी की पारंपरिक संस्थाओं को दिया गया संरक्षण शैव धर्म के पुनरुत्थान का कारण बना, लेकिन इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया।
आठवीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंश का उदय हुआ। वाराणसी को पुनः शैव धर्म का समर्थन मिला, क्योंकि ये शासक न केवल ब्राह्मणवादी थे, बल्कि शक्ति के तांत्रिक संप्रदाय के भी प्रबल अनुयायी थे। पाल वंश के शासन में वाराणसी की पारंपरिक भैरव-गण पूजा ब्राह्मणीय रूप और आत्मा के साथ समाहित हो गई।
916 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा इंद्रयुद्ध ने काशी पर अधिकार कर लिया। भारतीय इतिहास में राष्ट्रकूटों की स्थिति अस्पष्ट है, लेकिन वे शैव या शक्ति उपासना के समर्थक थे।
कुछ लोगों का मानना है कि वाराणसी के गाहड़वाल वंश के राजा राष्ट्रकूटों के वंशज थे।
1041 ईस्वी में गाहड़वाल वंश का आगमन हुआ, और उन्होंने 153 वर्षों तक (1015-1194) काशी पर शासन किया। यह अवधि अल्पकालिक थी, लेकिन वाराणसी ने इन गाहड़वाल राजाओं के शासनकाल में ऐतिहासिक उन्नति के अनेक सोपान तय किए।
आधुनिक वाराणसी का 80% स्वरूप वही है जो गाहड़वालों ने इसे बनाया था। इस 80% में से 50% अब भी काल के आघात को सहकर बचा हुआ है और लोककथाओं तथा स्मृतियों के रूप में सम्मान और प्रेम से याद किया जाता है।
III
इसके बाद उत्तर-पश्चिम से आई लूटपाटी सेनाओं द्वारा काशी पर विनाशकारी आक्रमण हुए, जिन्होंने एक पूरी तरह से अलग सैन्य तकनीक और भिन्न उद्देश्यों के साथ आक्रमण किया।
महमूद ग़ज़नी और उसके अनुयायियों का मुख्य उद्देश्य लूटपाट और विनाश था, और इसके लिए जो स्पष्ट बहाना बनाया गया वह था एकमात्र 'सच्चे' धर्म में परिवर्तन। विध्वंस और बर्बादी, लूट और आगजनी, हत्या और बलात्कार ने उनकी कामुक सेनाओं को निर्दोष नागरिकों पर वैसे ही टूट पड़ने के लिए उकसाया, जैसे टिड्डियाँ हरे-भरे खेतों पर टूट पड़ती हैं। पूरा भारत स्तब्ध था। पूरे उपमहाद्वीप की संस्कृति एक भयानक परिवर्तन के दौर से गुज़री।
इस समय समाज की निष्क्रिय मानसिकता के कारण पुनर्निर्माण कठिन हो गया। ब्राह्मणीय आचार संहिताएँ, कठोर जातिगत भेदभाव और संकीर्ण स्वीकृति की मानसिकता प्रभावी थी। एक बार जो 'अशुद्ध' या 'अपवित्र' हो गया, वह पुनः अपने समाज में नहीं लौट सकता था। 'अपवित्र' हिंदू न केवल समाज से बहिष्कृत होता, बल्कि उसे और भी कष्ट झेलने पड़ते।
सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सामाजिक संरचना स्थायी रूप से दो भागों में विभाजित हो गई। परिवार और रिश्तेदारों को केवल इसलिए त्याग दिया गया क्योंकि 'भेड़ियों' ने उन्हें छू लिया था। बहादुरों का सम्मान करने और उन्हें वापस अपनाने के बजाय, दुर्भाग्यशाली पुरुषों और महिलाओं को स्थायी बहिष्कार झेलना पड़ा।
परिणामस्वरूप, एक विशाल जनसमूह को शत्रु खेमे में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहाँ न केवल उन्हें सुरक्षा मिली, बल्कि सम्मान और न्याय भी प्राप्त हुआ।
तब जो विभाजन हिंदुओं और परिवर्तित लोगों के बीच उत्पन्न हुआ, वह आज तक मिटाया नहीं जा सका।
हालाँकि, जैन, बौद्ध और ब्राह्मणीय परंपराओं के बीच हुए धार्मिक संघर्षों ने भी मंदिरों, चैत्यगृहों और मठों को काफी क्षति पहुँचाई। चीनी विद्वान द्वारा वर्णित शिव की त्रिआयामी मानवाकार तांबे की मूर्ति, जिसमें जटाएँ, नाग और एक योगी का भव्य मुख था, यह सिद्ध करती है कि इसे लूटने का प्रबल आकर्षण था, क्योंकि यह बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित थी।
एक मानवाकार (मानव आकृति) त्रिआयामी शिव प्रतिमा के उल्लेख से कई बिंदु सामने आते हैं:
1. रुद्र-शिव या भरा-शिव जिस देवता की उपासना करते थे, वह एक प्रतीकात्मक पत्थर (शिला, गोल पत्थर, क्रिस्टल, या अनिश्चित आकार का उल्कापिंड) था। चूँकि हड़प्पा उत्खनन में इसी प्रकार के पत्थर मिले हैं और एक योगी जैसी आकृति भी पाई गई है, जिसके चारों ओर पशु और सर्प हैं और जो किसी प्रकार का मुकुट धारण किए हुए है, इसलिए इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इसे 'शिव-पशुपति' के रूप में व्याख्यायित किया। यह संभव है, लेकिन इसमें एक समस्या है।
यदि यह शिव की मूर्ति होती, तो यह अपनी तरह की अनूठी मूर्ति होती, जिसमें 'तीसरी आँख' का चिह्न नहीं है, न ही त्रिशूल या बाघ/हाथी की खाल जैसी पारंपरिक वेशभूषा।
लेकिन वाराणसी के भरा-शिव अभी भी प्रतीकात्मक लिंग रूप की पूजा करते रहे, जो आज भी वाराणसी के शिव मंदिरों और शैव परंपराओं में प्रचलित है।
2.
प्रतिमा रूप में देवता की अवधारणा गंधार-कुषाण काल (200 ईसा पूर्व – 320 ईस्वी) के
बाद ही अस्तित्व में आई। इसलिए ह्वेनसांग द्वारा वर्णित तांबे की मूर्ति इससे पहले की नहीं हो सकती।
3.
इसमें कोई संदेह नहीं कि तांबे की मूर्ति बहुमूल्य और आकर्षक थी। यह उन लुटेरों के लिए बहुत कीमती थी, जिनका
एकमात्र उद्देश्य लूटपाट था। उनके लिए तांबा दुर्लभ, महँगा और महत्वपूर्ण धातु थी।
जब हमें यह पता है कि महमूद ग़ज़नी का एकमात्र उद्देश्य लूटपाट था, न कि किसी स्थायी साम्राज्य की स्थापना, तो यह मानना कठिन नहीं है कि तांबे की यह मूर्ति उसी द्वारा या उसके एजेंट निआल्तगिन द्वारा लूटी गई। यह संभव है कि यह प्रतिमा निआल्तगिन की निजी विजय-ट्रॉफी बन गई (1033 ईस्वी)।
1001 ईस्वी में पुरुषपुर (पेशावर) में जयपाल को पराजित करने और 1021-22 ईस्वी में उसके पुत्र अनंगपाल की हत्या के बाद, हिंदू शाही वंश का अंत हो गया।
एक बार जब महमूद को हिंदुस्तान की अपार संपत्ति का स्वाद लग गया, तो उसने तब तक आक्रमण जारी रखा जब तक कि 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु नहीं हो गई। वह भारत पर शासन करने में कोई रुचि नहीं रखता था, जो कि विशुद्ध लुटेरों का एक विशिष्ट लक्षण है।
अपने लालच में अधिक से अधिक धन एकत्र करने के लिए, उसने अंततः भव्य वाराणसी पर आक्रमण किया और उसके सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए।
इसी समय उसे ग़ज़नी में अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला, और वह तुरंत वापस लौट गया। उसका डिप्टी निआल्तगिन विध्वंस जारी रखे रहा। 1034 ईस्वी में, वाराणसी के सभी प्रमुख मंदिर नष्ट कर दिए गए, जिनमें अविमुक्तेश्वर भी शामिल था, जो ब्राह्मणीय वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था और ज्ञानवापी के उत्तरी किनारे पर स्थित था।
इस लिंग के बारे में हम आगे भी सुनेंगे।
IV
1034 से 1192 तक वाराणसी को कुछ राहत मिली। इस अवधि में एक शक्तिशाली वंश ने वाराणसी पर शासन किया। 1018 में जब ग़ज़नी ने कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया, तो प्रतिहारी उत्तर और पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गए और संकटग्रस्त नगर पर किसी न किसी रूप में अपना नियंत्रण बनाए रखा।
विद्याधर चंदेल ने कन्नौज पर शासन करना शुरू किया, जबकि वाराणसी और प्रयाग पर 1039 ईस्वी में कलचुरी राजा गांगेयदेव का शासन था। उनके पुत्र कर्ण की मृत्यु 1070 में हुई।
1090 तक वाराणसी पर एक नया, मजबूत और दूरदर्शी शासक वंश शासन करने लगा। ये थे गाहड़वाल, एक अत्यंत शक्तिशाली वंश, जिसने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के बड़े भाग पर शासन किया। 1030 से 1090 के बीच वाराणसी को अविमुक्तेश्वर, जिसे विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, के बिना ही रहना पड़ा।
गाहड़वाल वंश के अधीन वाराणसी ने आधी सदी की निष्क्रियता के बाद पुनः समृद्धि पाई। वरुणा नदी के आसपास के सभी बाजार और दुकानें महमूद और निआल्तगिन द्वारा उजाड़ दी गई थीं। ओंकार, कृतिवास, आदि केशव, महाकाल, मध्येश्वर सहित सभी प्रमुख मंदिर धूल में मिला दिए गए थे। लूट अत्यंत व्यापक और पूर्ण थी। यहाँ तक कि अविमुक्तेश्वर (विश्वेश्वर), भवानी और ज्ञानवापी जैसे प्रमुख मंदिर भी बख्शे नहीं गए। ज्ञानवापी पहाड़ी पर स्थित स्वयंभू लिंग का विनाश लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात था। कुछ परंपरावादी इस बात पर अड़े थे कि एक बार यदि स्वयंभू लिंग खंडित हो जाए तो उसकी पुनः स्थापना नहीं की जा सकती, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए एक नया लिंग पुनः स्थापित किया गया।
गाहड़वालों के शासनकाल में इन सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया और इस महान नगरी की महिमा पुनः लौटने लगी। व्यापारियों और यात्रियों को फिर से वाराणसी आकर्षित करने लगी। गाहड़वालों के प्रभावी प्रशासन में वाराणसी फिर से समृद्ध हुई।
विश्वनाथ (जिसे विश्वेश्वर या अविमुक्तेश्वर भी कहा जाता था) और अन्य मंदिर पुनः जीवंत हुए।
लेकिन कालांतर में इस दूसरे मंदिर को भी अन्य आक्रमणों में नष्ट कर दिया गया। मंदिरों पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य अपार धन प्राप्त करना था।
V
1192 में, तराइन के दूसरे युद्ध में, अफगानिस्तान के मुहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर मार डाला। इस विजय के साथ उसे भारत में प्रवेश का मार्ग मिल गया। उसका उद्देश्य महमूद ग़ज़नी से भिन्न था। ग़ज़नी का मुख्य उद्देश्य केवल लूटपाट था, जबकि घोरी भारत में इस्लाम फैलाने और अल्लाह के नाम पर हिंदुस्तान को जीतने के इरादे से आया था। उसका उद्देश्य केवल लूटपाट तक सीमित नहीं था, बल्कि वह भारत को एक इस्लामी साम्राज्य में बदलना चाहता था।
1194 में, चंदावर के युद्ध में, गाहड़वालों का अंतिम शासक पराजित हुआ और वाराणसी पूरी तरह नष्ट कर दी गई। यह वाराणसी का दूसरा व्यापक विध्वंस था। केंद्रीय पहाड़ी पर फिर से बनाए गए विश्वनाथ मंदिर ने इस उग्र मूर्तिभंजक का विशेष आक्रोश झेला।
लेकिन इसमें एक चूक रह गई। हालाँकि उसने ज्ञानवापी के साथ-साथ मंदाकिनी क्षेत्र के गणपति मंदिरों, ओंकार, महाकाल, कालभैरव, मध्येश्वर मंदिरों को भी नष्ट कर दिया और इस प्रक्रिया में अपार धन प्राप्त किया, फिर भी वह यह सोचने की भूल कर बैठा कि उसने विश्वनाथ लिंग को नष्ट कर दिया है। उसने ऐसा नहीं किया। वह ऐसा कर ही नहीं सका। एक श्रद्धालु ब्राह्मण ने इसे ज्ञानवापी के जल में छिपा दिया था।
वाराणसी का दूसरा विध्वंस पूर्ण हो चुका था। केंद्रीय पहाड़ी पर स्थित मंदिर फिर से ध्वस्त कर दिया गया।
घोरी के दिल्ली के वायसराय कुतुबुद्दीन की 1192-93 में मृत्यु हो गई। इस समय वाराणसी का प्रशासन उसके एजेंट जमालुद्दीन द्वारा किया जा रहा था। उसका नाम आज भी वाराणसी में 'जमालपुरा' या 'जमालुद्दीनपुरा' के रूप में विद्यमान है।
इस हमले के बाद वाराणसी में बड़ी संख्या में धर्मांतरित लोग बस गए। आज भी जमालपुरा इन धर्मांतरितों के वंशजों से भरा हुआ है। फिर भी, धर्मांतरित हों या न हों, वे सच्चे वाराणसीवासी थे और आज भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। वाराणसी के प्रति उनका प्रेम उन्हें यहाँ की हस्तकला से गहराई से जोड़ता है।
VI
मानो खुले घावों पर नमक छिड़कने के लिए, कुतुबुद्दीन और उसके गवर्नरों ने हिंदू समुदाय को अपमानित करने के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई।
मंदिरों में अनेक कलात्मक वस्तुएँ थीं। विजेताओं की परिष्कृत दृष्टि उन कलात्मक वस्तुओं के उपयोगितावादी मूल्य को समझने में असफल नहीं हो सकती थी। कुतुबुद्दीन और उसके अधिकारियों ने आदेश जारी किए कि इन खंडहरों और उनके पत्थरों, स्तंभों, मेहराबों और द्वारों का उपयोग नई मस्जिदों के निर्माण में किया जाए। पूरे वाराणसी में नष्ट किए गए मंदिरों के अवशेषों से मस्जिदें बनाई जा रही थीं। इनमें अढ़ाई कंगूरे की मस्जिद अभी भी हिंदू कला के कुछ नमूने संरक्षित रखती है। (तुलना करें: अजमेर की अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद।)
दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर के निर्माण में भी इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, जहाँ अनंगपाल के निकटवर्ती सूर्य मंदिर के अवशेषों का उपयोग किया गया था। इसी प्रकार कई अन्य मस्जिदों का निर्माण इस काल में इसी विधि से किया गया।
वाराणसी के चौक क्षेत्र के पास आज भी ऐसी एक मस्जिद खड़ी है। दूसरी एक कबर्गाह मकदून शाह के नाम पर बनाई गई, जिसे सुंदर हिंदू स्तंभों से सजाया गया था। वाराणसी के गुलजार मोहल्ले में यह कबर्गाह अभी भी कला प्रेमियों के लिए हिंदू कारीगरों की उत्कृष्ट कारीगरी का प्रदर्शन करती है। (हमें उन गरीब कारीगरों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने गाहड़वालों के संरक्षण में ऐसी कला का सृजन किया था।)
लेकिन इस काल की एक अनूठी मस्जिद राजघाट के निकट स्थित है। आकार, भव्यता और स्थापत्य की उत्कृष्टता के मामले में यह उल्लेखनीय है, विशेष रूप से इसके आंतरिक सजावट और संरचनात्मक भव्यता के लिए, जो हिंदू मंदिरों से ली गई थी।
VII
खिलजी वंश के अला उद्दीन और उसके सेनापति मलिक काफूर ने हिंदू मंदिरों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने में विशेष सक्रियता दिखाई। उनकी लूट और विध्वंस की नीति कट्टरता से भरी थी।
इन विजेताओं की मानसिकता ने हिंदू समाज को स्थायी क्षति पहुँचाई। धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं को बिना किसी भय के कुचला गया। विजेताओं ने कभी भी जनता में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया, जिससे जनता सदैव असुरक्षित और आतंकित महसूस करती रही। प्रशासनिक दक्षता के लिए शासक का जनभावनाओं से जुड़ा होना आवश्यक होता है, लेकिन विजेताओं ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया।
हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण और उनकी महिलाओं के अपमान के कारण अपने ही परिवार और समाज से अलग कर दिया गया। इससे समाज में कोई समायोजन नहीं हो सका, बल्कि कटुता और संघर्ष को ही बल मिला।
हिंदू (जिसमें आदिवासी और मूल निवासी भी शामिल थे) सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को आत्मसात करते आए थे, लेकिन कट्टर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण यह समायोजन संभव नहीं हो सका।
गुलाम वंश (1210-1290) के निरंतर दरबारी षड्यंत्रों और सूफी विचारधारा के प्रसार ने मुस्लिम कट्टरवाद में कुछ नरमी के संकेत दिए। कट्टरता को दार्शनिक समझ की कोमलता ने थोड़ा नरम कर दिया। इस नए सूफी आंदोलन में अमीर खुसरो, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और सम्राट कैकोबाद जैसे नाम महत्वपूर्ण रहे।
इस परिवर्तन के साथ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक नए प्रकार की आपसी समझ विकसित होने लगी। वाराणसी ने इस बदलाव को विशेष रूप से अपनाया। परंतु यह भाईचारे की भावना लंबे समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अत्याचारी सम्राटों की नीतियों ने इसे फिर से नष्ट कर दिया।
दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में वाराणसी ने दमन से मुक्त होने का अंतिम प्रयास किया। लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1266-1296 के बीच इल्तुतमिश और कैकोबाद के शासनकाल में वाराणसी में जो मंदिर पुनर्निर्मित किए गए थे, उन्हें सुल्ताना रज़िया के आदेश पर फिर से ध्वस्त कर दिया गया।
इस विध्वंस का उद्देश्य दरबारी गुटों को प्रसन्न करना था, न कि रज़िया के अपने धार्मिक विश्वासों को लागू करना। परंतु इससे रज़िया को कोई लाभ नहीं हुआ। शरिया के विरुद्ध एक महिला शासक के अधीन कार्य करने को मजबूर दरबारी उसे हटाने के लिए तत्पर थे, और अंततः उसकी हत्या कर दी गई।
इसी अवधि में, अर्थात् इल्तुतमिश और कैकोबाद के समय, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत की गई, लेकिन इसे तीसरी बार नष्ट कर दिया गया।
हम इस काल के पुनर्निर्माणों के बारे में contemporary work 'प्रबंधकोष' से जानते हैं, जहाँ लेखक ने एक गुजराती व्यापारी वास्तुपाल को भगवान विश्वनाथ की सेवा के लिए 10,000 रुपये का दान देने के लिए धन्यवाद दिया है।
1296 से 1316 के बीच, अला उद्दीन खिलजी ने भी मंदिरों की लूट में अपार लाभ देखा। चूँकि उत्तर भारत के मंदिर पहले ही नष्ट किए जा चुके थे, इसलिए उसने दक्षिण भारत की ओर रुख किया, जहाँ के मंदिर अपार धन-संपदा से संपन्न थे।
इस अभियान में उसे उसके कुशल सेनापति मलिक काफूर का सहयोग मिला, जिसने कुंभकोणम, त्रिचूर, कांची, मदुरै, मैसूर, द्वारसमुद्रम जैसे मंदिरों और मंदिर-नगरियों को लूटा और ध्वस्त किया। यादव, होयसाल और पांड्य राजवंश समाप्त कर दिए गए। महान विजयनगर साम्राज्य भी अतीत का हिस्सा बन गया।
विश्वनाथ मंदिर चौथी बार ध्वस्त कर दिया गया, और इस बार इसे लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया गया।
फिर भी, यह आश्चर्यजनक है कि इसी समय ज्ञानवापी क्षेत्र में एक पद्म साधु ने एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसे 'पद्मेश्वर मंदिर' कहा गया। यह कैसे और कब बना, यह इतिहास की एक अनसुलझी पहेली है।
जौनपुर की लाल दरवाजा मस्जिद पर अंकित एक शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि "वाराणसी में, विश्वेश्वर मंदिर के पास, पद्म साधु ने एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसकी मीनारें हिमालय की चोटियों जितनी ऊँची थीं..."।
इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि:
1. पहाड़ी पर स्थित मंदिर स्थल को पूरी तरह से छोड़ दिया गया;
2. धमकियों के बावजूद वाराणसी के भक्तों ने मंदिरों का निर्माण जारी रखा;
3. पद्मेश्वर मंदिर संभवतः वर्तमान आदि विश्वेश्वर मंदिर के स्थान पर बनाया गया था।
बाद में यह क्षेत्र पूरी तरह से मलबे और कचरे से भर गया। नागरिकों ने इस ढेर को कूड़ेदान की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया। इस स्थान को 'कटवारखाना' (कचरा डंपिंग ग्राउंड) कहा जाने लगा, और आज भी यह नाम वर्तमान सत्यनारायण मंदिर के पास की एक संकरी गली में बना हुआ है।
इस दौरान वाराणसी को एक राहत मिली, जिससे इसे पुनर्निर्माण का अवसर मिला। दक्षिण की ओर विस्तार के कारण पुराने शहर से ध्यान हट गया, और वाराणसी फिर से पुनर्जीवित होने लगी।
VIII
फिरोज तुगलक (1359-88) ने भले ही शिक्षा और कृषि विकास के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया हो, लेकिन उसने 'काफ़िरों' और उनके धार्मिक संस्थानों के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई। उसके शासनकाल में पवित्र बकरिया (बकरि) कुंड को न केवल ध्वस्त कर दिया गया, बल्कि वहाँ के सुंदर मंदिरों के खंडहरों से प्राप्त सामग्री का उपयोग मस्जिदों के निर्माण में स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति दे दी गई। संपूर्ण कुंड, जिसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता था, मस्जिद का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया गया, जिससे यह स्पष्ट रूप से संरचना का एक अविनाशी अंग बन गया।
बकरिया कुंड के आसपास स्थित सभी प्रसिद्ध कलात्मक मंदिर पूरी तरह मिटा दिए गए, और आज यह स्थान पूरी तरह वीरान, भयानक और अत्यंत निराशाजनक दिखाई देता है।
यदि हम 1436-58 के बीच वाराणसी पर हुए आक्रमण को देखें तो तुगलकों का काल वाराणसी के लिए कुछ राहत का समय प्रतीत होता है। इस अवधि के दौरान जौनपुर के शासक, मोहम्मद शाह शर्की ने इस नगर पर आक्रमण किया। शर्की वंश तुगलक सुल्तानों द्वारा गवर्नर नियुक्त किए गए थे, लेकिन उन्होंने विद्रोह कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बाद में उन्हें पराजित कर बंगाल खदेड़ दिया गया, जहाँ उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। लेकिन इस बीच जौनपुर के शासक ने समृद्ध वाराणसी पर हमला किया और विश्वनाथ मंदिर को लूट लिया। इस पाँचवें विध्वंस ने विश्वनाथ मंदिर की तुलना में अविमुक्तेश्वर मंदिर को अधिक प्रभावित किया, जो ज्ञानवापी में स्थित पद्मेश्वर के पास प्रमुख देवता बन चुका था।
IX
चौदहवीं शताब्दी के दौरान वाराणसी का व्यापार फिर से समृद्ध हुआ, और व्यापारियों में एक नया सोने की होड़ देखी गई। दूर-दूर से लोग वाराणसी में बसने के लिए आने लगे, और जंगलों, नदियों, झीलों और आश्रमों से भरी घाटी ने अधिक विस्तार और निर्माण के लिए रास्ता बना दिया। यह विस्तार मंदाकिनी घाटी से लेकर उत्तर में वरुणा नदी के तटों तक सीमित था। सैकड़ों नए मंदिर उभर आए, और नई तीर्थस्थलों की महिमा का गान करने वाली पुस्तकें लिखी गईं। इस पूरे प्रभाव ने शहर को अत्यधिक भीड़भाड़ वाला बना दिया।
जनसंख्या में अचानक वृद्धि के साथ-साथ धूर्त और ठगों, व्यापारिक ब्राह्मणों और 'पंडा' या 'पांडव' नामक चालाक गाइडों की संख्या भी बढ़ी। विश्वनाथ मंदिर पहाड़ी की ढलानों पर अपनी पूरी भव्यता में खड़ा था। लेकिन ज्ञानवापी में स्थित अविमुक्तेश्वर को वाराणसी के सर्वोच्च देवता के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। विश्वेश्वर (या विश्वनाथ) और विशालाक्षी का स्थान गौण हो गया।
अविमुक्तेश्वर के पास प्रसिद्ध पद्मेश्वर मंदिर था, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। यह स्पष्ट है कि ऐसी प्रशंसाएँ बाद में जोड़ी गईं, क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से स्थापित एक असाधारण संरचना थी।
हालाँकि, इन धार्मिक ग्रंथों में जो स्तुतियाँ दर्ज हैं, वे एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा करती हैं। वाराणसी के प्रमुख देवताओं पर लिखी गई पुस्तकें अक्सर ब्राह्मण पुरोहितों के नियंत्रण में थीं, जो अनौपचारिक मंदिरों और नए देवताओं को शामिल करने के लिए नई रचनाएँ जोड़ने या बदलने में कोई संकोच नहीं करते थे। इससे न केवल नए देवताओं को पवित्र नगर में स्थान मिलता था, बल्कि इसके साथ आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होता था।
समय के साथ, विश्वनाथ और अविमुक्तेश्वर को समर्पित मूल्यवान चढ़ावे पूरे हिंदू भारत से आने लगे। मगध, बंगाल, गया, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्कन के शासकों और व्यापारियों ने नियमित रूप से वाराणसी को भेंट भेजनी शुरू की। चौदहवीं शताब्दी की शुरुआत तक वाराणसी की स्थिति व्यापारिक समृद्धि और बढ़ती जनसंख्या के साथ काफी बेहतर हो गई थी।
शहरी विस्तार हमेशा प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों की कीमत पर होता है। इसी समय महाजनटोला, कुंजरटोला, पक्की महल, मंगला गौरी, जगतगंज, इसरगंगी, नाते इमली, बिसेसरगंज, जतंवर, त्रिलोचन, नारियलटोला, दलमंडी, जैतपुरा आदि क्षेत्रों में घर और दुकानें बड़ी संख्या में बननी शुरू हुईं। जनसंख्या तेजी से शहर के दक्षिणी छोर की ओर बढ़ी, और पश्चिमी सीमाएँ उन लोगों से भर गईं, जिन्हें इस्लामी आक्रमणों ने विस्थापित किया था।
अन्य सभी विस्तारित शहरों की तरह, वाराणसी में भी झुग्गियाँ उभरने लगीं। लेकिन वाराणसी के हृदय स्थल में, इसकी झीलें और जलधाराएँ, मच्छोदरी और मंदाकिनी की महान झीलें और वरुणा के दोनों किनारों पर स्थित मानव बस्तियाँ अभी भी अपनी संपूर्णता में बनी रहीं। वाराणसी अभी भी अपने हरियाली पर गर्व कर रही थी।
हिंदू समृद्धि अधिक समय तक नहीं रह सकी। संग्रहीत धन ने लुटेरों को आकर्षित किया। धार्मिक पाखंड ने मानवता के विरुद्ध किए गए अमानवीय कार्यों को वैधता प्रदान करने के लिए एक आदर्शवादी बहाना उपलब्ध करा दिया।
इसलिए, वाराणसी पर दो लगातार आक्रमण हुए—पहला फिरोज शाह तुगलक द्वारा और दूसरा सिकंदर लोदी द्वारा।
पहाड़ी पर स्थित विश्वनाथ मंदिर, जिसे रज़िया की मस्जिद से बदल दिया गया था, हिंदुओं द्वारा पुनर्निर्माण के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। लेकिन प्रसिद्ध पद्मेश्वर मंदिर का अब केवल एक समूह ही शेष रह गया था, जो ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी छोर पर स्थित तीन कब्रों का एक मंच है। यहाँ, कभी-कभी कोई अकेला श्रद्धालु एक दीप जलाता है, या शिवरात्रि की रात एक पुष्पगुच्छ रख जाता है, जिसे कट्टर निगाहों से बचाकर रखा जाता है।
लेकिन यह सौ वर्ष व्यर्थ नहीं गए। हिंदुओं ने इस्लामी कट्टरता से अपने मौलिक भेद को पहचाना, जो केवल कुरान और शरीयत तक सीमित थी। इसके विपरीत, हिंदू एक सर्वोच्च चेतन शक्ति में विश्वास रखते थे, जो सभी जीवन रूपों को प्रेरित करती थी। यह सार्वभौमिक अवधारणा सहस्राब्दियों में विकसित हुई थी, जिसमें भारत में आने वाले विभिन्न मतों और आस्थाओं को आत्मसात करने की क्षमता थी।
यह व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण, यद्यपि उदार और सार्वभौमिक था, फिर भी इसमें वह कठोर एकता और ठोस संगठन नहीं था, जो किसी समुदाय को संघर्ष के समय आवश्यक होती है।
1526 से 1747 तक मुगलों का शासन रहा, लेकिन बाबर और हुमायूँ ने वाराणसी को विशेष रूप से परेशान नहीं किया। 1559 तक वाराणसी को अकेला छोड़ दिया गया था। हालाँकि, विश्वनाथ या अविमुक्तेश्वर मंदिरों का कोई पुनर्निर्माण नहीं हुआ था। पूरी एक पीढ़ी इस प्रतीक्षा में थी कि कोई उद्धारकर्ता आएगा। लेकिन महान हिंदू एकता कभी भी एक जादुई मिश्रण में परिवर्तित नहीं हो सकी, और अंत तक यह बौद्धिक वाद-विवाद में ही विभाजित रही।
13.सदियों की नृत्यगाथा
I
जब पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया (1526), तब हिंदू भारत इस संघर्ष में विशेष रुचि नहीं रखता था। उनकी आत्मकेंद्रित दृष्टि में यह मात्र एक इस्लामी सीमा-संघर्ष प्रतीत हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अन्य लोगों को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। इस युद्ध में हिंदुओं की भागीदारी महज एक औपचारिकता थी या फिर एक अनिवार्य राजनीतिक दायित्व। हिंदुस्तान के हृदय ने इस संघर्ष के प्रति कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अंततः कोई भी विदेशी शासन हिंदू हितों के लिए शुभ नहीं होगा। उन्होंने बस यह इच्छा जताई कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को समाप्त कर दें। शायद वे यह भी मानते थे कि एक हड़पने वाले की जगह दूसरे का आ जाना हिंदुओं के लिए बेहतर होगा।
जनता को इस संघर्ष की कोई विशेष चिंता नहीं थी। वे जानते थे कि चाहे खान हो, राव हो या सिंह, उनके लिए उत्पीड़न ही उनका भाग्य था। भूख का कोई नाम या पंथ नहीं होता।
राजनीतिक चेतना या राष्ट्रीय पहचान जैसे अमूर्त विचारों ने भारत की आत्मा को कभी भी उद्वेलित नहीं किया था। जनता दिल्ली या सिरहिंद में खेली जा रही इस नाटक में कोई रुचि नहीं रखती थी। भारत में एक सांस्कृतिक एकता अवश्य थी, जो उसकी प्राकृतिक सीमाओं से भी परे फैली हुई थी, लेकिन राष्ट्रवाद की कोई अवधारणा तब तक उभर कर नहीं आई थी, न ही भारत में और न ही विश्व में। यदि हिंदू चेतना ने कहीं प्रतिक्रिया दी भी, तो भी एक साझा मातृभूमि या एक झंडे के प्रति निष्ठा की कोई भावना नहीं थी।
खेतीहर मजदूरों का एक बड़ा वर्ग जानता था कि अंततः उन्हें ही इस संघर्ष में पीसा जाना है, चाहे जीत किसी की भी हो। आर्थिक न्याय या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर दोनों पक्ष समान रूप से खतरा थे—चाहे 'खान' की जीत हो या 'राजपूत' की। आम जनता को इसमें कोई ऐसी 'भावना' नहीं मिली जिसके लिए वे अपने प्राणों की आहुति दें।
उन्होंने स्वयं को दिल्ली के इस नाटक से अलग ही रखा। यदि मंदिर-लूटने वाले उन्हें परेशान नहीं करेंगे, तो almighty राजाओं के कर-संग्राहक निश्चित रूप से करेंगे। मंदिर और कर-संग्रह दोनों ही उनके लिए वैसे ही थे जैसे शिकारी कुत्ते उनके मांस के पीछे पड़े हों।
संक्षेप में, जनता ने किसी राष्ट्रीय संकट या व्यक्तिगत खतरे की भावना को महसूस ही नहीं किया। उनके लिए संकट तो उनके जीवन का हिस्सा था।
एकमात्र संभव एकता का स्रोत धार्मिक समुदाय की भावना हो सकती थी। धर्म को व्यक्तिगत अस्तित्व का अभिन्न अंग माना जाता था। गरीबों और असहायों के लिए एक अंतिम सहारा एक सर्वोच्च शक्ति में उनकी गहरी आस्था थी—एक अदृश्य दिव्य न्याय। जितना गरीब और असहाय कोई व्यक्ति होता, उसकी धार्मिक आस्था उतनी ही अधिक मजबूत होती। सांस्कृतिक पहचान की अस्पष्ट भावना ने उनमें एक ऐसी एकजुटता उत्पन्न की, जैसी कि चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, तिलचट्टे, कौवे या बंदर आपसी स्वभाव से बना लेते हैं। ईश्वर व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता कर सकता था, लेकिन संगठित धर्म या एक संगठित धार्मिक मोर्चे की अवधारणा भारतीय मानस में अकल्पनीय थी। एक हिंदू के धार्मिक पहचान की पूरी अवधारणा में यह व्यक्तिगत अपील निहित थी। यदि कोई संकट उत्पन्न होता, तो जनता पुरोहितों की ओर देखती, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वही राजकुमार और चतुर पुरोहित उनके शोषक रहे हैं और भविष्य में भी शोषण करते रहेंगे।
यह प्रतिक्रिया इतनी व्यक्तिगत, अंतरंग और आरक्षित थी कि कोई भी सामुदायिक उत्तर उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता था। यहां तक कि यदि हिंदू अपनी पुरातन विरासत के प्रति किसी सामुदायिक भावना से प्रेरित होते भी, तो भी उसमें वह शक्ति नहीं थी जो एक बिखरी हुई भीड़ को संगठित कर सके और किसी साझा खतरे के विरुद्ध खड़ा कर सके। उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था कि उनके राजकुमार या पुरोहित किसी भी युद्ध के बाद उनके समर्थन में खड़े हुए हों। आम जनता को या तो युद्ध की तैयारी में योगदान देना पड़ता था, या फिर युद्ध में हार या जीत की कीमत चुकानी पड़ती थी। वे हमेशा खेल के कमजोर पक्ष में ही होते थे।
जोश की कमी थी। आर्थिक अनिच्छा को हिंदू दार्शनिक प्रवृत्ति ने और अधिक कमजोर कर दिया, जो कि किसी स्पष्ट सामूहिक आस्था के सिद्धांत से बचती थी। कुछ नकारात्मक पहलुओं में बहुसंख्यक सहमत हो सकते थे, लेकिन सकारात्मक विश्वासों में समाज पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्भर था।
स्वाभाविक रूप से, तथाकथित नेताओं के दावों के विपरीत, धर्म राजनीतिक खतरे का विरोध करने में एक कमजोर भूमिका निभाता था। अलग-अलग, और अक्सर विरोधाभासी, धार्मिक तर्कों के कारण, हिंदुओं का एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध उतना ही खड़ा होता था, जितना कि वे किसी अन्य धर्म के विरुद्ध होते थे। यदि हिंदू किसी गोमांस-भक्षी समुदाय के साथ भोजन या विवाह नहीं कर सकते थे, तो वे अपने ही हजारों समुदायों में भी ऐसा नहीं कर सकते थे। हिंदू एकता हजार दरारों से बिखरी हुई थी।
एकजुटता की भावना हिंदुओं की विदेशी आक्रमणों के प्रति प्रतिक्रिया में पूरी तरह अनुपस्थित थी। यदि कभी कुछ प्रतिष्ठित नेता इस खंडित मोज़ेक में विश्वास भरने में सक्षम भी हुए, तो ऐसे व्यक्तिगत महिमामंडित अध्याय अपवाद ही थे, न कि नियम।
इसलिए पानीपत का पहला युद्ध हो या दूसरा, गज़नी हो या गौरी, बाबर हो या सांगा—इनमें से कोई भी घटना भारतीय उपमहाद्वीप या उसके निवासियों के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी। ऐसा कोई भी महान कारण नहीं था जो उग्र प्रतिरोध को संगठित कर सके या किसी साझा खतरे के विरुद्ध समर्पित मोर्चे का निर्माण कर सके। सामंतवाद में युद्ध हमेशा स्थानीय स्तर पर लड़े जाते थे।
II
बहलोल लोदी के बाद 1489 में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। इस्लाम के प्रति लोदी उत्साह ने सिकंदर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान को इस्लामीकरण केवल एक कट्टर नीति को जारी रखकर और हिंदू धर्म के केंद्रों, विशेष रूप से मंदिरों को नष्ट करके ही किया जा सकता है। वाराणसी के मंदिरों पर उसका हमला व्यापक था। उसकी लूट की मात्रा अत्यधिक थी।
जब तक लोदी वंश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तब तक विश्वनाथ मंदिर का तीसरा पुनर्निर्माण हो चुका था, जिसे सिकंदर लोदी ने 1494 में ध्वस्त कर दिया। 1494 से 1594 तक, ऐसा प्रतीत होता है कि वाराणसी को बिना किसी विश्वनाथ मंदिर के रहना पड़ा।
जब 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई और बाबर ने दिल्ली की सत्ता संभाली, तब महान प्रायद्वीपीय भारत अपनी विलासिता की गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाबर और उसके बाद हुमायूँ, दोनों अपने लिए एक साम्राज्य स्थापित करने में व्यस्त थे। उनके लिए फरगना की वापसी, जिसे वे छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे, लगातार लड़ने वाले कबीले संघर्षों की ओर लौटने जैसा था। इसके विपरीत, भारत की अपार संपत्ति और विशालता उनके लिए अत्यधिक आकर्षक थी।
बाबर, जिसकी तीव्र अंतर्दृष्टि ने उसे भारत में विभाजित समाज की स्थिति से अवगत कराया, वह यहाँ रुकने और अपने लाभों को दृढ़ करने के लिए लड़ा। बाबर में सेनापतित्व के गुण राजनीतिक अवसरों की धारणा और अटूट महत्वाकांक्षा से सशक्त थे।
बाबर के जीवन की एक घटना उसके प्रसिद्ध संस्मरणों में अच्छी तरह से वर्णित है। जो सरदार बाबर के साथ आए थे, उन्होंने लंबे समय तक अपने देश से दूर रहने के कारण 'पैतृक भूमि' लौटने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। वे निरंतर युद्ध से इतने थक चुके थे कि उन्हें इसकी समाप्ति असंभव लग रही थी।
अलेक्जेंडर के सैनिकों में भी इसी तरह का मनोभाव उत्पन्न हुआ था, जिससे उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। लेकिन बाबर की प्रकृति भिन्न थी।
इसके अलावा, बाबर की शक्ति उसकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता के बराबर थी। उसने वापस जाने से इंकार कर दिया। अपने संस्मरणों में वह अपने अनिच्छुक साथियों को भारत की समृद्धि, संभावनाओं और एक महान और सुसंपन्न भूमि पर विजय प्राप्त करने के सपने के बारे में बताता है। "तुलना में शुष्क तुर्किस्तान तुम्हें क्या दे सकता है, जबकि यह भूमि दूध और शहद की नदियों से भरी हुई है?" उसने उनसे पूछा।
इस साक्ष्य से स्पष्ट है कि बाबर केवल एक आक्रमणकारी नहीं था, बल्कि एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध था। पिता और पुत्र दोनों, बाबर और हुमायूँ, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहे। वे यहाँ टिकना और निर्माण करना चाहते थे। प्रतिमाओं को नष्ट करना उनके विजय अभियान में प्राथमिकता नहीं रखता था।
वे इस अल्लाह-प्रदत्त अवसर को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे कि वे एक ऐसे देश में एक राजवंशीय साम्राज्य स्थापित करें, जहाँ अनेक विभाजन थे लेकिन कोई एकता नहीं, अनेक संधियाँ थीं लेकिन कोई सुरक्षा नहीं।
फिर भी, उसने भी मंदिरों को गिराने का प्रयास किया। अयोध्या का मंदिर इसका एक उदाहरण है। लेकिन वाराणसी ने उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि उसके समय में वाराणसी में कोई महत्वपूर्ण मंदिर नहीं था जिसे लूटा जा सके।
अपनी विजय के फलों को अपने बेटों में बाँटने की उसकी योजना सफल नहीं हुई। 'कभी हार न मानने वाले' अफगानों, जिनके पास शेरशाह जैसा एक शक्तिशाली नेता था, के कारण हुमायूँ लगभग अपना साम्राज्य खो बैठा था, और वास्तव में वह इसे छोड़ भी देता, यदि उसके दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी की एक दुर्घटनावश हुई मृत्यु उसे बचा न लेती।
1538 में, शेरशाह सूरी के आदेश पर वाराणसी में एक सामूहिक नरसंहार हुआ, लेकिन यह हत्या केवल मुगल सैनिकों और उनके प्रति वफादार लोगों तक ही सीमित रही। हिंदुओं को अकेला छोड़ दिया गया।
जब अकबर ने शासन की बागडोर संभाली, तो उसने स्वयं वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण शहर का प्रशासन अपने हाथ में लिया। लेकिन उसने भी अपने इस्लामी पूर्ववर्तियों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों, विशेष रूप से वाराणसी के मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए कोई विशेष पहल नहीं की।
इस सबका परिणाम यह हुआ कि सामान्य हिंदू और विशेष रूप से वाराणसी को एक राहत मिली। धर्म प्रचार के नाम पर मूर्तिभंजन, लूट, बलात्कार और आतंक के युग को थोड़े समय के लिए विराम मिला। वाराणसी ने राहत की सांस ली।
हुमायूँ, जब 1530 में जौनपुर के विद्रोही अफगानों को पराजित करने के लिए निकला, तो उसे सारनाथ के उजाड़ जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। क्योंकि जौनपुर जाने का रास्ता वाराणसी से होकर नहीं गुजरता था, उसने शहर का दौरा नहीं किया। सारनाथ के पास आधुनिक सड़क के किनारे स्थित अष्टकोणीय लाल ईंट की संरचना आज भी उसके शिविर स्थल को चिह्नित करती है।
1494 से 1580 तक, इस्लामी कट्टरता से वाराणसी को कुछ राहत मिली। किसी के पास इसे नुकसान पहुँचाने का समय नहीं था। अकबर ने 1556 में वाराणसी का दौरा किया और मिर्जा रज़वी और शेरशाह सकरीवाल को इस महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर का संयुक्त राज्यपाल नियुक्त किया।
लेकिन अकबर की इस्लामी शासक के रूप में प्रशिक्षण को संतुलित किया गया था। उसने 'भारतीय' शासक बनने को प्राथमिकता दी। समझदार और उदार सलाहकारों द्वारा निर्देशित, उसने धीरे-धीरे एक परिपक्व राजनेता के रूप में उदार विचार अपनाए। इस संदर्भ में उसके सर्वश्रेष्ठ सलाहकार अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, बीरबल, भगवंदास और मान सिंह थे, जो सभी दूरदृष्टि रखने वाले कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भविष्य की ओर देखा और एक कुशल प्रशासन के आधार पर साम्राज्य को संगठित किया।
वह भारत में पहले इस्लामी शासक थे, जिन्होंने यह स्वीकार किया और सराहा कि भारत ही उनका घर है और भारतीय जनता ही उनके अपने लोग हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली अंग्रेज भी इस अवधारणा के अनुसार शासन करने में असफल रहे और इस कारण वे साम्राज्यवादी असंवेदनशीलता के शिकार हुए। अकबर ने स्वयं को पहले एक शासक और बाद में एक मुस्लिम माना।
III
इस प्रकार वाराणसी ने एक स्वागत योग्य विराम का अनुभव किया। लेकिन इस विराम का अर्थ यह भी था कि नए मंदिरों का निर्माण या पुराने मंदिरों की मरम्मत का प्रयास नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप, वाराणसी लगभग सौ वर्षों तक विश्वनाथ मंदिर के बिना बनी रही। (वाराणसी पहले ही ओंकार, कृतिवास, कालेश्वर, अविमुक्तेश्वर, मध्यमेंश्वर आदि मंदिरों के बिना रहने की आदत डाल चुकी थी।)
1545 से 1554 के बीच, अपने पिता के आदेश पर, वाराणसी सीधे अकबर के अधीन थी, लेकिन 1555 में हुमायूँ ने अपने पुत्र से शासन वापस ले लिया। 1556 में एक दुर्घटना में हुमायूँ की मृत्यु हो गई, और अकबर सिंहासन पर बैठा।
इतिहास गवाह है कि अकबर को अपनी स्थिति को स्थिर करने में कुछ समय लगा, खासकर राजा हेमचंद्र (हेमू) के कड़े विरोध का सामना करने के बाद और फिर अपने गुरु बैरम खान को चतुराई से दरकिनार करने के बाद। इन शुरुआती चुनौतियों को पार करने में उसे अंबर राजघराने का बहुत सहयोग मिला।
उसने अपने दरबार के हिंदू लॉबी का आभार व्यक्त किया, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि हिंदू पुनरुत्थान की किसी भी संभावना पर उसकी नजर बनी रहे। फिर भी, वाराणसी में सभी जगह मंदिरों का निर्माण फिर से शुरू हो गया।
1580 तक, वाराणसी (और भारत) के हिंदू समुदाय को एक विद्वान ब्राह्मण नारायण भट्ट से लाभ हुआ। उनकी कई पुस्तकें अब भी उपलब्ध हैं। इनमें से एक "तीर्थ कल्पतरु" पहले ही उल्लेखित की जा चुकी है।
उन्होंने टोडरमल को सलाह दी कि वे अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था के प्रति शिक्षित करें, खासकर एक ऐसे देश में जिसने मानव इतिहास के कुछ सबसे प्राचीन धर्मों को पोषित, आश्रय और विकसित किया था।
अगर अकबर सफल और लोकप्रिय सम्राट बनना चाहता था, तो उसे सही शासकीय स्वभाव को अपनाना और अभ्यास करना आवश्यक था। उसे एक उदार और दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाना था और यह साबित करना था कि वह भारत की भूमि के एक केंद्रीय सम्राट के रूप में एक मजबूत, न्यायप्रिय और उदार नीति का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसे यह सिद्ध करना था कि वह अपने सभी प्रजा के लिए न्यायसंगत है। वह अपनी ही आस्था के अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में बहुसंख्यक हिंदू जनता की उपेक्षा नहीं कर सकता था।
मुगलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती, आश्चर्यजनक रूप से, हिंदुओं से नहीं आई। यह चुनौती उनके सहधर्मी पठानों से आई, जिन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत से प्राप्त प्रभुत्व को अवसरवादी 'विदेशियों', अर्थात चीन के तुर्किस्तान से आए असफल और नापसंद मुगलों द्वारा हड़प लिया गया है।
मजबूत पठान-अफगान राजवंश पहले से ही भारत के गुजरात, बंगाल और दक्कन के बड़े हिस्सों में स्थापित थे। इन सबने युवा सम्राट के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की।
एक ही धर्म के समुदायों के बीच यह खूनी संघर्ष इस सिद्धांत को झूठा साबित करता है कि अंतर-सामुदायिक युद्ध धर्म के मतभेदों पर आधारित थे। धर्म को केवल एक छलावा के रूप में उपयोग किया गया था ताकि चालाक स्वार्थी लोग साधारण लोगों में उन्माद पैदा कर सकें, जो वास्तव में सत्ता और लालच के लिए होने वाले युद्धों में मानव संसाधन प्रदान करते थे।
इस शक्तिशाली चुनौती को पार करने के लिए अकबर को हिंदुओं का सहयोग अत्यंत आवश्यक था। अगर हिंदू अफगानों के साथ मिल जाते, या अपने हितों की रक्षा के लिए सम्राट के प्रयासों को विफल कर देते, तो यह मुगलों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता।
हिंदुओं ने सम्राट को महत्वपूर्ण सुरक्षा और सहयोग प्रदान किया। टोडरमल की सलाह और बिहारीमल द्वारा अपनी बेटी के विवाह की पेशकश—जिसमें उनकी अपनी शर्तें थीं, ताकि अकबर की हिंदू नीति की वास्तविकता साबित हो—ने युवा सम्राट को इस नीति की बुद्धिमत्ता को समझने में मदद की। उसने जोधाबाई, बिहारीमल की बेटी से बड़े धूमधाम से विवाह किया। इस हिंदू राजकुमारी को हरम में सर्वोच्च स्थान दिया गया, और उनका पुत्र राजसिंहासन का उत्तराधिकारी बना।
इस नई नीति ने युवा सम्राट को एक महान राजनीतिक लाभ दिया, क्योंकि उसके मंत्रिमंडल में प्रभावशाली हिंदू घरानों के प्रमुख शामिल थे, जो भारत के सबसे योग्य और श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक ‘मस्तिष्क केंद्र’ बन गए, और इस तरह के प्रतिभाशाली और सर्वश्रेष्ठ लोगों का समर्थन प्राप्त करने वाले वह भारत के सबसे योग्य मुस्लिम सम्राट बन गए।
इस बुद्धिमानी भरे कदम ने हिंदुओं और नापसंद किए गए पठानों के संभावित गठबंधन को रोका। अकबर को हिंदू जनता के प्रति अपनी न्यायसंगत नीति में एक सच्चा विश्वास जगाने की सख्त जरूरत थी।
इसके विपरीत, पठानों की हिंदू नीति, यहां तक कि इल्तुतमिश, मुहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे शिक्षित शासकों की भी, कभी भी हिंदू जनता का विश्वास नहीं जीत सकी। पठानों को हमेशा 'विदेशी' माना जाता था क्योंकि वे हिंदू-विरोधी माने जाते थे।
इसका कारण यह था कि अफगानों द्वारा निर्मित इस्लामी व्यवस्था कट्टरपंथी कठोर मौलवियों के एक समूह से जुड़ी हुई थी। उनके रूढ़िवादी प्रभाव भूमि के शासक के उदारवादी निर्देशों से अधिक महत्वपूर्ण साबित हुए। दिल्ली की एकमात्र महिला शासक, रजिया सुल्ताना का पतन इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। मौलवी गुट हमेशा दिल्ली की उदार नीति के रास्ते में सीधे बाधा बनकर खड़ा रहा और हिंदू बहुसंख्यकों का वांछनीय विश्वास जीतने में अप्रत्यक्ष रूप से विफल रहा।
अगर औरंगजेब मौलवी गुट के बजाय दारा शिकोह की धर्मनिरपेक्षता की महान सिद्धांत को अपनाता, तो वह अपने वंश और हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकता था?
IV
युवा अकबर ने शीघ्र ही यह समझ लिया कि अपने पूर्ववर्तियों की कट्टरता से सीखना बुद्धिमानी होगी; और यही उसकी महानता के आधार के रूप में स्थापित हुआ। अकबर ने सम्राटीय नीति के तहत खुद को मौलवियों के प्रभुत्व से मुक्त कर लिया।
जब भी कोई चुनौती सामने आई, तब भी कैकोबाद, इल्तुतमिश, मुहम्मद तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक जैसे विद्वान शासक, स्थानीय गवर्नरों की तरह ही संकीर्ण मानसिकता के साथ कार्य करने लगे। दरबारी साजिशों और दबावों के कारण वे कट्टरता के आगे झुक गए।
जौनपुर का पठान गवर्नर, मुहम्मद शर्की, इसका एक उदाहरण था। वह केवल एक उपाधिधारी शासक था, लेकिन उसने खुद को एक कट्टर उन्मादी के रूप में प्रस्तुत किया, जो केंद्रीय नीति की परवाह किए बिना अपने मनमाने ढंग से कार्य करता था।
इन सहायक गवर्नरों के इस अंधे जोश और मौलवियों द्वारा बढ़ाए गए उनके अत्याचारों ने हिंदू मानस को उस विश्वास से पूरी तरह दूर कर दिया, जिसे एक केंद्रीय सत्ता से प्राप्त किया जा सकता था।
अकबर ऐसी नीतियों के प्रतिकूल प्रभाव से सतर्क था। इसके बजाय, उसे इस्लामी शासन की तथाकथित न्यायप्रियता में एक स्थायी विश्वास को बढ़ावा देने की सलाह दी गई थी। वह एक केंद्रीय दिल्ली-शक्ति स्थापित करना चाहता था, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करे, और यह शासन मौर्यों, गुप्तों और कुषाणों के हिंदू शासन की याद दिलाए।
अकबर ने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की, जो एक केंद्रीय सरकार के अधीन हो, जहां राजस्व की स्पष्ट और स्थायी व्यवस्था हो, और किसानों को स्थानीय सामंतों के मनमाने करों से मुक्ति मिले। उसने अभियुक्तों को लंबी और दमनकारी न्यायिक प्रक्रियाओं से बचाने का प्रयास किया। उसने अपने प्रजा के किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की नीति अपनाई।
अकबर कोई पारंपरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति नहीं था। बचपन में उसे शांति से अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला। वह एक ऐसा व्यक्ति था, जो जॉन स्टुअर्ट मिल की तरह बचपन से वंचित था। वह अति-लाड़-प्यार में पला, जिद्दी, कठोर और पूर्ण निरंकुशता की सीमा तक दृढ़ संकल्पी था।
लेकिन उसमें एक अद्वितीय प्राकृतिक प्रतिभा थी, जिसके कारण उसने अपने दरबार में एक मेधावी मंडली (जैसे विक्रमादित्य के समय और बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के दरबार में) एकत्रित की, जिससे उसने बहुत कुछ सीखा।
इस मेधावी मंडली में सबसे विश्वसनीय व्यक्ति थे राजा टोडरमल, रूपांतरित संगीतज्ञ मियां तानसेन, राजा बिहारीमल के पुत्र राजा भगवानदास, जिनकी बुआ जोधाबाई का विवाह अकबर से हुआ था। जोधाबाई ही आगे चलकर अगले सम्राट जहांगीर की माता बनीं।
इस प्रकार, अकबर भारत में पहले मुस्लिम शासक बने, जिन्होंने हिंदू जनता पर शासन करने की बुद्धिमानी को समझा और उन्हें अनावश्यक रूप से उकसाने की नीति को त्याग दिया।
इस नीति की दूरदर्शिता उनके कर सुधारों में परिलक्षित हुई, जिसमें उन्होंने हिंदुओं पर लगाए गए कई भेदभावपूर्ण करों को समाप्त कर दिया। इस उदार नीति से राजकोष को अधिक लाभ हुआ, और निश्चिंत हिंदुओं ने उसे अफगान सरदारों—जैसे मालवा, गुजरात और दक्कन के मुस्लिम शासकों से निपटने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान किया।
अकबर की हिंदू नीति में इस पूर्ण परिवर्तन ने हिंदुस्तान में मुगलों की पकड़ को मजबूत किया।
इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, और भारतीय राजनीति की गहरी समझ के कारण, अकबर ने हिंदुओं को कई अनुदान जारी किए। उसने हिंदुओं पर लगाए गए अपमानजनक तीर्थ-कर को समाप्त कर दिया, और उससे भी अधिक घृणास्पद जज़िया कर को हटा दिया, जिसे शरीयत के अनुसार किसी गैर-मुस्लिम से लिया जाना अनिवार्य था।
इस तरह की उदार नीति की सिफारिश उनके दार्शनिक गुरु अब्दुल लतीफ ने की थी, जिन्होंने उन्हें "सुलह-ए-कुल" (सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति) अपनाने की सलाह दी थी। इससे पहले किसी अन्य मुस्लिम शासक ने इस नीति को इतनी गहराई से नहीं अपनाया था, और न ही इसके बाद किसी ने इसे इतनी दृढ़ता से लागू किया।
जब अकबर युवा था और उसके सोचने-समझने की उम्र थी, उसने उन ताकतों को सख्ती से कुचल दिया जो उसे मौलवियों के नियंत्रण में रखना चाहती थीं। उसकी कठोर, तत्काल और दृढ़ कार्रवाई ने सभी विरोधों को दबा दिया। उसने अपनी धाय मां के बेटे, एक विद्रोही अधिकारी, को केवल अपनी मुट्ठी से मार डाला, क्योंकि वह हत्या की साजिश रच रहा था।
अकबर ने अपनी "सुलह-ए-कुल" नीति को प्रारंभ में ही निर्धारित कर लिया था। यह कानून-ए-शरीयत के खिलाफ जाने और मौलवियों के विरोध का सामना करने के लिए एक युवा राजकुमार के लिए अत्यधिक साहस का कार्य था।
यही कारण था कि उसने वाराणसी के खंडहर हो चुके मंदिरों और अन्य ध्वस्त तीर्थस्थलों के पुनर्निर्माण का आदेश दिया।
राजनीति की इस अनूठी रणनीति ने पूरे हिंदू भारत में विश्वास की लहर उत्पन्न कर दी। इससे पहले कभी भी हिंदुओं को किसी विदेशी शासक से इतनी प्रोत्साहना नहीं मिली थी।
अब अकबर को हिंदू विरोध की चिंता नहीं थी। वह अब अपने चारों ओर मौजूद आक्रामक और शक्तिशाली अफगान विरोध पर ध्यान केंद्रित कर सकता था।
सदियों से, अफगान यह मानते आए थे कि भारत उनका जायज अधिकार है। वे इतनी आसानी से अपनी कठिनाई से अर्जित सत्ता को इन ट्रांस-ऑक्सस (फरगना के पार) के 'साहसी' मुगलों के हाथों खोने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्हें वे केवल अवसरवादी लुटेरों के रूप में देखते थे।
महान मुगल अकबर को अब यह साबित करना था कि वह वास्तव में उसी भूमि का उत्तराधिकारी था, जहाँ उसका जन्म हुआ था।
अगर अकबर ने कट्टरवाद के निरर्थक आग्रहों को छोड़कर अपनी उदार नीति से जनता को अपने पक्ष में नहीं किया होता, तो वह विश्व इतिहास के महानतम शासकों में से एक नहीं माना जाता।
V
1580 में अकबर ने बिहार के अफगानों को मुँगेर में अंतिम और निर्णायक हार दी। यह एक मनोवैज्ञानिक रूप से उपयुक्त क्षण था। प्रभावशाली दरबारियों जैसे भगवंदास और टोडरमल के सहयोग से, चतुर और विद्वान ब्राह्मण नारायण दत्त ने एक योजना बनाई। उन्होंने इस अवसर का उपयोग अकबर को वाराणसी के पुनर्निर्माण की आवश्यकता और महत्व को समझाने के लिए किया।
प्राचीन वरुणा क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और उसकी पुनर्बहाली लगभग असंभव थी। फिर भी, 'महान पाँच' मंदिरों और बिंदुमाधव मंदिर का आंशिक पुनर्निर्माण किया गया। लेकिन गंगा के किनारे की पहाड़ियों को विकसित किया जा सकता था, और पूरे एक नए शहर का मॉडल हिंदुओं के लिए आनंद का विषय बन सकता था। सम्राट इस एकल निर्णय से संपूर्ण राजवाड़ा और संभवतः मराठवाड़ा को भी एकजुट कर सकते थे। नारायण दत्त ने अकबर को इस रणनीतिक कदम की बुद्धिमत्ता से अवगत कराया।
सिकंदर लोदी ने 1494 में वाराणसी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, और 1580 में अकबर ने इसके सामान्य पुनर्निर्माण की अनुमति दी। हिंदू प्रजा के प्रति अपनी कृपा को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए, सम्राट ने स्वयं विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए 45,000 स्वर्ण दिनारों का अनुदान दिया।
एक बार जब सम्राट की इस उदारता की घोषणा हुई, तो भारत के अमीर और गरीब, हिंदू राजकुमारों और धनी व्यापारियों ने इस परियोजना में धन की वर्षा कर दी।
वाराणसी ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने सभी संसाधनों को संगठित किया। पहले से ध्वस्त किए गए कई मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया।
पंडित नारायण दत्त अत्यंत सक्रिय हो गए। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादियों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि म्लेच्छों द्वारा अपवित्र किए गए स्थलों के पुनः उपयोग की परंपरागत निषेधाज्ञा को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने धार्मिक शास्त्रों का हवाला देते हुए समाज को यही समझाने की कोशिश की कि वे उन्हीं स्थानों पर नए मंदिरों का पुनर्निर्माण करें।
पंडित के मार्गदर्शन में, कृतिवासेश्वर, महाकालेश्वर, मध्येश्वर और ओंकारेश्वर मंदिरों का उनके मूल स्थानों पर पुनर्निर्माण किया गया, जो पहले उजाड़ और वीरान पड़े थे।
इस पुनर्निर्माण में, अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर मंदिर को प्राथमिकता दी गई।
VI
अब तक विदेशी आक्रमणकारियों ने वाराणसी के उन मुख्य मंदिरों को लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जो वरुणा नदी और दो झीलों—मंडाकिनी और मच्छोदरी—के बीच स्थित थे। यह क्षेत्र वाराणसी का हृदय स्थल था और यहाँ के मंदिर इसकी समृद्धि के प्रतीक थे। विध्वंस पूरी तरह से संपन्न किया गया था।
इसलिए, इन सभी मंदिरों को एक साथ पुनर्स्थापित करना असंभव था। अतः, पंडित नारायण दत्त ने यह बुद्धिमानी समझी कि वे अपने प्रयासों को ज्ञानवापी और उसके समीप के क्षेत्र तक सीमित रखें।
लेकिन यह क्षेत्र भी, जैसा कि हमने पहले देखा, एक बदबूदार, गंदा, और भयानक मलबे का ढेर बन चुका था। सदियों से जमा हुई गंदगी ने इसकी प्रसिद्ध सुंदरता, भव्यता और पवित्रता को पूरी तरह नष्ट कर दिया था।
पंडित नारायण दत्त के लिए ज्ञानवापी का पुनर्निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने पहाड़ी पर स्थित रज़िया मस्जिद की जाँच की और समझ गए कि उसे छूना असंभव होगा। अतः, पहाड़ी पर मंदिर बनाने की योजना तुरंत छोड़ दी गई।
दूसरा सबसे उपयुक्त स्थान था ज्ञानवापी के दक्षिणी किनारे पर, जहाँ एक ओर कभी अविमुक्तेश्वर मंदिर स्थित था, और दूसरी ओर प्रसिद्ध अक्षयवट वटवृक्ष था।
लेकिन यह क्षेत्र भी मलबे से भर चुका था। वास्तव में, यह गंदगी ढलान के साथ नीचे बहकर ज्ञानवापी के जल-क्षेत्र तक आ गई थी और इसे लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था।
शिल्पकारों ने योजना बनाई कि इस गंदगी को हटाकर इसे सड़क के स्तर तक लाया जाए, जो तब पहाड़ी पर स्थित रज़िया मस्जिद तक पहुँचती थी। इतिहास में दर्ज है कि नव-निर्मित मंदिर का मंच सड़क के स्तर तक ऊँचा किया गया। (आज भी यह मंच देखा जा सकता है।)
हालाँकि, ज्ञानवापी अपनी पूर्व जलराशि को पूरी तरह पुनः प्राप्त नहीं कर सका। वह झील, जिसकी सतह स्वर्ण-शिखरों वाले मंदिरों का दर्पण की तरह प्रतिबिंब दिखाती थी, हमेशा के लिए अवरुद्ध हो गई।
एक और कारण हो सकता है कि विश्वनाथ मंदिर को अन्य अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों की तुलना में पहले बनाया गया।
प्राचीन नगर और व्यावसायिक केंद्र राजघाट-मच्छोदरी-वरुणा क्षेत्र से और दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गए थे। आबादी अब वरुणा और मंडाकिनी की दक्षिणी सीमा की ओर बढ़ रही थी। सारनाथ पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया था।
इस प्रकार, पहाड़ी पर स्थित मंदिर अब नगर के केंद्र के अधिक निकट हो गया था।
ज्ञानवापी की तरह, मच्छोदरी भी अत्यधिक प्रदूषित हो गई थी, जिससे जलमार्ग का उपयोग कठिन हो गया। नए व्यापार मार्ग अब स्थलीय रास्तों के साथ विकसित हो गए, जो वाराणसी को गौर और पांडुआ जैसे समृद्ध नगरों से जोड़ते थे।
इसलिए, मच्छोदरी और विश्वनाथ पहाड़ी के दक्षिणी तट के बीच का क्षेत्र वाराणसी का सबसे व्यस्त केंद्र बन गया।
संभवतः यही कारण था कि नारायण दत्त ने अविमुक्तेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और विश्वनाथ लिंग को इसके केंद्रीय गर्भगृह में स्थापित किया।
पुनर्निर्माण के दौरान, वाराणसी के प्रसिद्ध पितृ-तीर्थ बकरी कुंड (बकरियाकुंड) को भी पुनर्स्थापित किया गया। इस कुंड को इतना अधिक महत्व दिया गया कि पूरे भारत के हिंदू राजकुमारों ने इसकी परिक्रमा में सुशोभित मंदिरों का निर्माण करवाने में होड़ लगा दी।
इन मंदिरों को उत्कृष्ट कलात्मक खंभों और सुंदर नक्काशीदार चित्रों से सजाया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मूर्तिकार यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे।
यह अत्यंत दुखद है कि नगर के प्रशासकों (और पूर्व ब्रिटिश कलेक्टरों) की घोर लापरवाही के कारण इस भारतीय कला के संग्रहालय को नष्ट कर दिया गया। यह अद्वितीय संपदा अवैध लूटपाट, मस्जिदों की सजावट, निजी भवनों, और प्रभावशाली लोगों की सनक को पूरा करने के लिए नष्ट कर दी गई।
मंडाकिनी तालाब के तट पर, जो उस समय सक्रिय था और मंडाकिनी चैनल से जल प्राप्त करता था, दो मंदिरों को स्थापित किया गया:
1. दंतहस्त गणेश मंदिर, जिसे "बड़ा गणेश" के नाम से जाना जाता है।
2. गोरक्ष टिला पर एक मंदिर, जहाँ प्रसिद्ध नाथ योगी जलंधरनाथ की समाधि स्थित है।
इस स्थान को अब भी ध्यानपूर्वक रखा जाता है।
तालाब के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर आज भी इसके अवशेष मौजूद हैं। वहीं, उत्तर-पश्चिमी किनारे पर मसालों का एक बाज़ार—कटरा दीननाथ—बसा था।
कटरा के पास, मैदागिन के समीप एक देवी मंदिर भी स्थित था।
इसी काल में नया कालभैरव मंदिर भी पुनर्निर्मित किया गया, क्योंकि पुराना मंदिर पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था।
VII
हम अब तक सत्रहवीं शताब्दी में विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की चर्चा कर रहे थे।
लेकिन अकबर की उदार स्वीकृति ने न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सौंदर्यीकरण की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इस महान नगर की शोभा बढ़ी।
मानसिंह और टोडरमल इस शाही अनुमति का यथासंभव शीघ्र और कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए तत्पर थे। उनके प्रयासों का परिणाम आज भी एक भव्य नदीतट के रूप में खड़ा है, जिसकी सुंदरता वेनिस, पोटोमैक या हांगकांग से भी अधिक अनुपम है। (इस पर आगे चर्चा की जाएगी।)
अल्प समय में ही संपूर्ण हिंदू भारत को सतर्क कर दिया गया, और विभिन्न राजाओं की सद्भावना नदी किनारे तीव्र निर्माण कार्यों के रूप में मूर्त रूप लेने लगी।
अकबर की राजनीति, सौंदर्य, सहिष्णुता और उदारता की स्थायी गौरव-गाथा के रूप में वाराणसी के नदी किनारे को कीचड़ भरी, उबड़-खाबड़ और ढीली मिट्टी की दीवारों से मुक्त किया गया। इसे तराशे हुए बलुआ पत्थरों, दृढ़ स्तंभों, सुंदर छतों और भव्य स्थापत्य कला से बने एक के बाद एक स्तरीय मंदिरों और महलों से सुसज्जित किया गया, जो क्रमशः ऊँचाई पर उठते हुए आकाश को भेदते प्रतीत होते हैं।
यह स्मरण करना सुखद है कि वाराणसी के नदी-तट की प्रसिद्धि इसी अद्वितीय भव्यता के कारण है।
यह भी याद रखना आवश्यक है कि इस सौंदर्य का श्रेय उस सम्राट को जाता है, जिसने अपनी प्रजा के हृदयों को जीतने का प्रयास किया और धर्म को व्यक्तिगत विषय माना, जबकि शासन को एक सार्वजनिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा। जो वास्तव में धार्मिक होते हैं, वे नैतिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, न कि पुरोहितों द्वारा थोपे गए कठोर नियमों का।
केदार घाट से पंचगंगा घाट तक, वाराणसी में गंगा का अर्धचंद्राकार प्रवाह विश्वभर के पर्यटकों, भक्तों, वास्तुकारों, फोटोग्राफरों, चित्रकारों और कवियों के लिए आश्चर्य, श्रद्धा और सराहना का केंद्र बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इस अनुपम निर्माण को नमन करता है।
हम इस अद्भुत सौंदर्य का बार-बार उल्लेख कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि वाराणसी के घाटों की अलौकिक शोभा का जितना वर्णन किया जाए, उतना ही कम प्रतीत होता है।
भारत में ताजमहल को सही रूप में एक आश्चर्यजनक उपलब्धि माना जाता है। उसी प्रकार वाराणसी के घाट भी प्रशंसा के योग्य हैं, जिन्हें न तो प्राचीन और न ही आधुनिक यात्रियों ने सराहे बिना छोड़ा है।
दूरदर्शी पर्यटक और यात्री, जो सदियों से वाराणसी आते रहे हैं, इसकी भव्य हिंदू स्थापत्य कला की प्रशंसा करते रहे हैं, जो अब भी अपनी दिव्य चमक से लोगों को आकर्षित करती है, चाहे निकट संपर्क से इस नगर की कुछ अस्वच्छताएँ भी उजागर क्यों न हो जाएँ।
वेन्स, जो अपने ऊँचे जलतटों के लिए प्रसिद्ध है, या लंदन, जो टेम्स नदी के किनारे फैली अपनी इमारतों के लिए जाना जाता है, वे भी वाराणसी के अर्धचंद्राकार घाटों की उस अद्वितीय बनावट की तुलना में फीके पड़ जाते हैं, जो शांतिमय सोपानों के माध्यम से धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए आकाश को आलिंगनबद्ध कर लेती है।
एक के बाद एक व्यवस्थित सैंडस्टोन की सीढ़ियाँ, चमकदार पत्थरों से सुसज्जित महलों और गुंबदों तक पहुँचती हैं। इन सीढ़ियों के किनारे-किनारे हरियाली से घिरी बालकनियाँ लगभग दो किलोमीटर तक पहाड़ी श्रृंखला के साथ चलती हैं। यह दृश्य मानवीय आकांक्षाओं की एक ठोस अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, जो सूर्य की किरणों में निखरकर साकार प्रतीत होती हैं। वाराणसी के घाटों का यह भव्य परिदृश्य वास्तव में मानवीय प्रार्थनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति है, जिसे मनुष्य असहाय होकर 'दैवीय शक्ति' कहता है। वाराणसी के नदीतट की सीढ़ियाँ पत्थरों में ढली हुई उस दिव्य आत्मा की स्तुति का प्रतीक हैं।
सौंदर्य और रोमांच से परे, इन सैकड़ों सीढ़ियों को पहाड़ियों के शिखर से बहती हुई गंगा की गहराइयों तक इस तरह से जोड़ना, कि उनकी मज़बूती को कोई ताकत हिला न सके, आज के आधुनिक मानकों से भी एक आश्चर्यजनक इंजीनियरिंग उपलब्धि है।
जो भी व्यक्ति उदयपुर और पिछोला झील, या राजस्थान के विभिन्न 'सागर' (विशाल तटबंधों) को देख चुका है, जो भव्य महलों से घिरे हुए हैं, वह वाराणसी के पहाड़ियों को जोड़ने वाले पत्थरों की संरचना की बारीकी को अवश्य समझ सकता है। इन ढीले पत्थरों को लोहे के क्लैंपों और सीसे के साँचे से इस तरह से मजबूती दी गई थी कि पूरी पहाड़ी श्रृंखला एक ठोस संरचना के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसे समय भी नहीं मिटा सका, और न ही प्रकृति उसे हिला पाई।
यह सब वाराणसी, या काशी-कोसल के उन कुशल राजमिस्त्रियों और पत्थर तराशने वाले शिल्पियों की कारीगरी का प्रमाण है, जिन्हें स्थानीय रूप से 'संतरास' कहा जाता था। ('संग' = पत्थर, 'तराश' = गढ़ना, इस प्रकार संगतराश या संतारास = पत्थर के कारीगर)। ये अपने आप में एक विशिष्ट वर्ग थे, जो आज भी अपनी पारंपरिक कला को दिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं।
इनकी प्रतिभा का उपयोग राजस्थान के राजाओं, महाराष्ट्र के शासकों और दक्षिण के राजवंशों ने भी किया। ये दक्षिण के शासक बाद में आए, लगभग एक शताब्दी बाद, लेकिन सम्राट अकबर की उदार नीति ने राजवाड़ा के राजाओं को संगठित किया, जिससे उन्होंने अपने सर्वोत्तम प्रयासों को अंजाम दिया और इस अप्रत्याशित शाही राहत का भरपूर लाभ उठाया।
सदियों बाद, हिंदू एक संगठित परिवार की तरह उठ खड़े हुए और वाराणसी का पूरा स्वरूप ही बदल दिया।
मिथकीय इतिहास में जिसे वाराणवती या वाराणस्य के नाम से जाना जाता था—जो कभी वरुणा नदी का सामना करता था—अब वह शहर गंगा की विशाल रेतीली तटरेखा की ओर मुख करने लगा। जो नगर कभी राजघाट, ऋषिपत्तन, और मच्छोदरी व मांडाकिनी के व्यस्त बाजारों के लिए प्रसिद्ध था, वह अब अपने प्राचीन मूल को भुलाकर सीधा गंगा की ओर मुख कर बैठा, और प्रत्येक सुबह उगते हुए सूरज का स्वागत करने लगा, जो पूर्वी तट की हरियाली से झाँकता हुआ रामनगर पर प्रकाश बिखेरता है।
आज (1990) हम जो भी गंगा तट पर देखते हैं, वह वर्षों की मानव-श्रम और संकल्प की परिणति है। यह भव्यता एक ही बार में नहीं आई, बल्कि चरणबद्ध तरीके से विकसित हुई। यदि वाराणसी की पहाड़ियाँ कभी घने जंगलों से आच्छादित थीं, यदि इन पहाड़ियों की भव्य हरियाली के कारण इसे आनंदकानन कहा जाता था, और यदि दूसरी ओर नदी के उजाड़ तटों को महाश्मशान के नाम से जाना जाता था, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन नगर मुख्यतः वरुणा नदी के दक्षिणी किनारों से सटा हुआ था और वर्तमान विश्वेश्वरखंड के बाहर स्थित नदी के घाटों से इसका कोई विशेष संबंध नहीं था। आधुनिक नगर तो मात्र प्राचीन तपोवनों का विस्तार है, जिसे साधुओं और ऋषियों ने बसाया और विकसित किया।
प्राचीन काल में पहाड़ी क्षेत्र भवनों से रहित था, क्योंकि वहाँ मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। यह निषेधाज्ञा शायद गणों के भय के कारण रही होगी।
इसीलिए नदी तट पूरी तरह से किसी भी शहरी सजावट से मुक्त था। यहाँ-वहाँ, भस्म से भरे, पशुओं से भरे, अंत्येष्टि स्थलों के सन्निकट बिखरी हुई बस्तियाँ थी, जहाँ भार-शिव, गुह्यक, यक्ष, गण और अंत्येष्टि करने वाले विभिन्न समुदाय बसे हुए थे। इनका अधिकांश जीवन घुमंतू कबीलाई जीवन जैसा था।
जिस भव्यता की आज हम सराहना करते हैं, वह तभी संभव हो सकी जब पहाड़ियों का शहरीकरण हुआ। जैसे-जैसे शहर का विस्तार हुआ, लोगों ने नदियों का उपयोग करना शुरू किया। स्वाभाविक रूप से, नदी तक पहुँचने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ी, जिसे दानशील समृद्ध राजाओं ने उपलब्ध कराया।
इस प्रकार, सबसे पहले सीढ़ियाँ और भवन संभवतः गौतम बुद्ध के समय के बाद ही निर्मित हुए, और कनिष्क के समय तक इन पहाड़ियों पर बस्तियाँ पूरी तरह विकसित हो चुकी थीं।
फिर भी, उस समय के अभियंताओं (इंजीनियरों) की क्षमता इतनी नहीं थी कि वे इतने भव्य घाटों का निर्माण कर पाते, जैसा कि हम आज देखते हैं।
हम अब तक सत्रहवीं शताब्दी में पुनर्निर्मित विश्वनाथ मंदिर की चर्चा कर रहे थे।
लेकिन अकबर की उदार स्वीकृति ने वाराणसी के सौंदर्यीकरण के संदर्भ में एक और भी महत्वपूर्ण और कलात्मक उद्देश्य को पूरा किया।
मानसिंह और टोडरमल इस शाही अनुमति का अधिकतम लाभ उठाने में अत्यंत तेज और चतुर सिद्ध हुए। और जो कुछ उन्होंने हासिल किया, वह आज भी एक अद्वितीय जलतट के रूप में खड़ा है, जिसकी तुलना न तो वेनिस से की जा सकती है, न पोटोमैक से, और न ही हांगकांग से। (इस पर बाद में चर्चा करेंगे।)
अल्प समय में ही संपूर्ण हिंदू भारत को सतर्क कर दिया गया, और राजाओं की सद्भावना ने एक तीव्र निर्माण गतिविधि के रूप में ठोस रूप लिया, जो नदी के किनारे स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी।
अकबर के राजनीतिक विवेक, सौंदर्यबोध, सहिष्णुता और उदारता की अनंत महिमा के लिए, वाराणसी के नदी तट को कीचड़, ढहते किनारों और अस्थिर चट्टानों से मुक्त किया गया, और इसे तराशे हुए बलुआ पत्थरों, दृढ़ स्तंभों, ऊँचे छज्जों और उत्तम शिल्पकला वाले मंदिरों तथा महलों से सुसज्जित किया गया, जो एक के ऊपर एक उठते हुए आकाश को छूने लगे।
यह स्मरण करना आनंददायक है कि वाराणसी के घाटों की प्रसिद्धि उस सम्राट की उदारता से उत्पन्न हुई, जिसने अपने प्रजा का हृदय जीतने की इच्छा रखी थी और जिसने धर्म को व्यक्तिगत विषय माना, न कि शासन के सार्वजनिक दायित्व के रूप में। सच्चे धार्मिक व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, न कि पुरोहितों द्वारा निर्धारित कठोर नियमों का।
केदार घाट से पंचगंगा घाट तक, वाराणसी में गंगा की अर्धचंद्राकार धारा विश्व भर के पर्यटकों, श्रद्धालुओं, स्थापत्यविदों, फोटोग्राफरों, चित्रकारों और कवियों के लिए विस्मय, प्रशंसा और श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। प्रत्येक अपने-अपने पसंदीदा माध्यम में इस अद्वितीय मानवीय उपलब्धि को नमन करता है।
हमने इस अद्भुत सुंदरता की चर्चा पहले भी की है और बार-बार करते रहेंगे, क्योंकि वाराणसी के घाटों का यह सौंदर्य पुनरावृत्ति के योग्य है।
भारत में ताजमहल को एक अद्भुत स्थापत्य उपलब्धि के रूप में सही रूप में सराहा जाता है। इसी प्रकार, वाराणसी के घाट भी प्रशंसा के पात्र हैं, जिनकी सुंदरता का वर्णन प्राचीन और आधुनिक यात्रियों ने समान रूप से किया है।
समझदार पर्यटक और यात्री, सदियों से, हिंदू वास्तुकला के इस भव्य दृश्य की प्रशंसा करते आ रहे हैं, जो आज भी अपनी चमक बरकरार रखता है, भले ही वाराणसी के निकट संपर्क से जो सqualor (गंदगी और अव्यवस्था) प्रकट होती है, वह इसकी आभा को कुछ हद तक फीका कर देती हो।
राजघाट, ब्रह्म घाट, दुर्गा घाट, बिंदुमाधव घाट, मंगलागौरी घाट, राम घाट, त्रिलोचन घाट, अग्नेश्वर घाट, नागेश्वर घाट (जो अब भोंसला घाट के नाम से जाना जाता है), वीरेश्वर घाट, सिद्ध विनायक घाट, स्वर्गद्वार प्रवेश, मोक्षद्वार प्रवेश (दोनों अब लोकप्रिय मणिकर्णिका घाट परिसर में सम्मिलित हो गए हैं), जरासंध घाट (बाद में मीर घाट के नाम से जाना गया, मीर रुस्तम अली, एक मुस्लिम कलेक्टर, के नाम पर, जिसने यहाँ एक छोटे किले जैसी संरचना बनवाई थी, जिसके अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं), बुद्धादित्य घाट, सोमेश्वर घाट (एक अन्य सोमेश्वर घाट, जो और दक्षिण में स्थित था, अब पर्रे या पांडेय घाट के नाम से जाना जाता है), रामेश्वर घाट (जो मान मंदिर के पास स्थित था), लोलार्क घाट (जो अब लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए जल-आपूर्ति भवनों के कारण समाप्त हो चुका है), असी संगम घाट (जो उत्तरी वरुणा संगम घाट के समान संतुलन बनाए हुए था, दोनों ही घाटों तक पक्के रास्ते नहीं थे)।
दशाश्वमेध घाट पहले से मौजूद था, साथ ही प्रयाग घाट भी। लेकिन घोड़ा घाट के पुनर्निर्माण के बाद इसका स्वरूप बदल गया। इस परिवर्तन को वास्तव में प्रशासनिक अधिकारियों की तत्परता ने संभव बनाया, जो विशेष रूप से श्वेत 'पर्यटकों' को नदी तट तक आसान (और कम असुविधाजनक) पहुँच प्रदान करने के इच्छुक थे।
पांडेय घाट के पास एक सर्वेश्वर घाट भी था, लेकिन यह अब पुरानी खंडहरों के मलबे में दफन हो चुका है। समान रूप से दुखद स्थिति मानसरोवर घाट की भी है। अकबर के दरबार के राजा मान सिंह ने प्राचीन मानसरोवर को पुनर्स्थापित किया था और इस जलाशय को चारों ओर से छतयुक्त बरामदों से सजाया था। इस जलाशय के चारों ओर चार मंदिर थे, और एक मंदिर बीच में स्थित था। अब यह सब मात्र एक स्मृति बनकर रह गया है। यह उल्लेखनीय है कि इस जलाशय के साथ-साथ दर्जनों अन्य जलाशयों का विनाश उन्हीं हिंदुओं द्वारा किया गया, जो आज भी कई और जलाशयों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता ने इस विनाश को और अधिक प्रोत्साहित किया।
केदार घाट बहुत पुराना है, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप मुगल काल में दिया गया था। केदार घाट के पास स्थित कुमारस्वामी मठ अकबर के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था।
केदार घाट के साथ ही, कई अन्य घाटों का उल्लेख गोविंदचंद्र, गहड़वाल वंश के राजा, के एक अभिलेख में मिलता है। यह दर्शाता है कि गहड़वाल शासक पहाड़ी वाराणसी को सजाने के प्रति सचेत थे। उन्होंने पहाड़ियों की ऊँचाइयों से नदी तक जाने के लिए अच्छी तरह से निर्मित रास्तों की व्यवस्था की। लोलार्क, आदिकेशव, वेदेश्वर, कोटितीर्थ (कपिलधारा के पास), त्रिलोचन और स्वप्नेश्वर (केदार घाट के समीप) के अलावा, गहड़वाल शासकों ने लोलार्क और विश्वनाथ जैसे मंदिरों तथा स्नानकुंडों के रखरखाव के लिए भी व्यापक प्रबंध किए।
अकबर और जहांगीर की उदार नीतियों से नाराज होकर, कट्टरपंथी मुल्लाओं ने शाहजहाँ से आग्रह किया कि वे इस्लाम की महिमा के अनुरूप एक कठोर नीति अपनाएँ और "काफिरों" पर कड़ा रुख अपनाएँ। शाहजहाँ ने एक फरमान जारी किया कि जो मंदिर पहले से बने हुए थे, वे बने रह सकते हैं, लेकिन जो मंदिर निर्माणाधीन थे, उन्हें न केवल रोका जाना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।
शाहजहाँ के शासनकाल में उनके सबसे बड़े पुत्र, दारा शिकोह, को इलाहाबाद का गवर्नर नियुक्त किया गया। वाराणसी उनके प्रशासन के अधीन आई। चूंकि दारा शिकोह हिंदू दर्शन में अत्यधिक रुचि रखते थे, उन्होंने वाराणसी को अपने निवास के रूप में चुना और इस विषय का गहन अध्ययन किया, जो उन्हें अत्यधिक प्रिय था। जिस क्षेत्र में वे रहते थे, वह बाद में "दारा नगर" के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उन्होंने यह क्षेत्र सोच-समझकर चुना, क्योंकि यह प्रसिद्ध कृतिवासेश्वर मंदिर के निकट स्थित था। इसलिए यह हिंदू दर्शन के विद्वानों का प्रमुख केंद्र भी था। लेकिन इसके बाद कट्टरपंथी मुगल सम्राट औरंगज़ेब का शासन आया, और वाराणसी को पहले से कहीं अधिक पीड़ा झेलनी पड़ी। और इसी के साथ, मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी हो गई।
मुगल साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से दो नीतियों के कारण हुआ:
1. औरंगज़ेब की धार्मिक नीति
2. उनकी दक्षिण नीति (दक्षिण भारत में आक्रमण)
समय के साथ युवा औरंगज़ेब ने "दारा-कॉम्प्लेक्स" विकसित कर लिया था। यह मानसिकता विशेष रूप से उसके पिता शाहजहाँ द्वारा अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अधिक महत्व देने और अन्य बेटों की उपेक्षा करने के कारण उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा, दारा शिकोह की पत्नी (उदयपुरी) की सुंदरता को लेकर भी औरंगज़ेब असंतुष्ट था और उसे यह स्वीकार नहीं था कि "एक विधर्मी" ऐसी सुंदर पत्नी का स्वामी बने।
यही कारण था कि औरंगज़ेब दारा के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगा, विशेष रूप से उसके दार्शनिक विचारों को लेकर, जो अकबर की नीति और दीन-ए-इलाही से प्रेरित थे। चूंकि औरंगज़ेब ने अंततः दारा शिकोह को "ईशनिंदा" के आरोप में मृत्युदंड दे दिया, यह अपेक्षित था कि वह कट्टरपंथी बन जाएगा, मुल्लाओं के समर्थन से हिंदुओं को कुचलने का प्रयास करेगा और दारा नगर, कृतिवास, वाराणसी और हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेगा।
औरंगज़ेब ने साबित करने के लिए कि वह इस्लाम की रक्षा और प्रचार में गंभीर है, कठोर कदम उठाए, जिनमें मंदिरों का विध्वंस भी शामिल था। वह यह दिखाना चाहता था कि वह दूसरे, तीसरे और चौथे मुगलों (अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ) की "भूलों" को सुधारने के लिए कटिबद्ध है।
इस प्रयास में, उसने वाराणसी में मंदिरों के पुनर्निर्माण को पूरी तरह से रोक दिया और निम्नलिखित मंदिरों को ध्वस्त कर दिया:
● विश्वनाथ मंदिर (नारायण दत्त द्वारा पुनर्निर्मित)
● अविमुक्तेश्वर
● कृतिवास
● ओंकार
● महाकाल
● मध्यमेश्वर
● बकरारी कुंड
● पंचगंगा घाट का प्रसिद्ध बेनीमाधव मंदिर
इस विध्वंस के कारण वाराणसी, जो सौ वर्षों तक अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थी, फिर से आहात हो उठी। यहाँ तक कि छोटे-छोटे मंदिर और जलाशय भी बर्बाद कर दिए गए। संपूर्ण मच्छोदरी-मandakini क्षेत्र खंडहर में बदल गया।
इस भयानक विध्वंस के कारण वाराणसी के लोगों में एक सामाजिक बदलाव देखा गया। इस्लाम के प्रति जो घृणा पहले केवल विदेशी आक्रमणकारियों तक सीमित थी, वह अब संस्थागत रूप लेने लगी। मंदिरों से अपहृत लड़कियों और जबरन धर्मांतरित हिंदुओं ने अपने पुराने समाज से खुद को अलग-थलग पाया और धीरे-धीरे हिंदू विरोधी मानसिकता विकसित कर ली।
लेकिन औरंगज़ेब, हालाँकि धार्मिक रूप से कट्टर था, एक कुशल शासक भी था। जब उसे लगा कि वह राजपूतों और मराठों की बगावत से घिर गया है, उसने अपनी नीति में थोड़ा बदलाव करने का संकेत दिया। वह अपने अत्यधिक उत्साही अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहता था।
इसके प्रमाण के रूप में, 28 फरवरी 1659 को जारी औरंगज़ेब का एक फरमान उल्लेखनीय है…
शरीयत के नियमों के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि वाराणसी के पुराने मंदिरों को बनाए रखा जा सकता है, लेकिन कोई नया मंदिर नहीं बनाया जाएगा। मेरी सरकार को सूचित किया गया है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने वाराणसी और उसके आस-पास के लोगों, विशेष रूप से उन ब्राह्मणों, जो मंदिरों में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, के लिए समस्याएँ खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। वे उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहते हैं। यह फ़रमान जारी किया जा रहा है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और भविष्य में उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन लोगों के पूजा-अर्चना के अधिकार बाधित न हों।
इस संदर्भ में यह याद रखना आवश्यक है कि 1659 में कृतिवास मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और उसी वर्ष उसकी जगह आलमगिरी मस्जिद बनाई गई थी।
दिल्ली में औरंगज़ेब की साजिशपूर्ण कैद से शिवाजी की चतुराई से बच निकलने के बाद, औरंगज़ेब का हिंदुओं के प्रति आक्रोश पूर्ण रूप से प्रकट हुआ और उसने भयानक विध्वंस किए।
सितंबर 1669 में विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया गया और एक फ़रमान जारी किया गया, जिसके अनुसार वाराणसी के संस्कृत विद्यालयों को बंद करने और सभी हिंदू ग्रंथों को जलाने का आदेश दिया गया। (दारा-शिकोह के प्रति ईर्ष्या और द्वेष ने हिंदू ग्रंथों और शिक्षाओं के विरुद्ध एक अभियान चला दिया था।)
इसके बाद बिंदुमाधव मंदिर की बारी आई। इस प्रसिद्ध मंदिर के स्थान पर एक नई मस्जिद बनाई गई, और इसकी मीनारें वाराणसी शहर के लिए प्रमुख स्मारक बन गईं।
यह मंदिर इतना भव्य था कि गंगा के तट पर ऊँचाई पर स्थित इसकी अद्वितीय शोभा को देखते हुए यहाँ तक कि ईसाई यात्रियों ने भी इसके विध्वंस की निंदा की। वे इस्लामी कट्टरता द्वारा एक सुंदर रचना को नष्ट किए जाने से स्तब्ध थे।
मूल बिंदुमाधव मंदिर में अत्यंत सुंदर मीनारें थीं और इसका मुख्य गर्भगृह स्वर्ण मंडित था। जब इस मंदिर को ध्वस्त किया गया और एक मस्जिद के रूप में इसे चुनौती देने की योजना बनाई गई, तो उतनी ही भव्य मीनारें बनाई गईं। गंगा के किनारे बनी औरंगज़ेब की मस्जिद की मीनारें लंबे समय तक वाराणसी के प्रतिष्ठित स्मारक बनी रहीं, लेकिन समय के साथ वे ढह गईं। (अब ये मीनारें अस्तित्व में नहीं हैं, समय ने इन्हें नष्ट कर दिया है।)
औरंगज़ेब के शासनकाल में वाराणसी और संपूर्ण भारत की सामाजिक स्थिति को दो फ्रांसीसी यात्रियों, फ्रांसिस बर्नियर और जीन फ्रांसिस टेवरनियर ने अपने यात्रा वृतांतों में बहुत अच्छे से वर्णित किया है। दोनों ही वाराणसी के व्यापार, विशेष रूप से इसके रेशम उद्योग की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।
हम उनके प्रति विशेष रूप से आभारी हैं क्योंकि उन्होंने उल्लेख किया कि वाराणसी का मुख्य शहर गंगा के उत्तरी किनारे पर स्थित था। इसका अर्थ यह हुआ कि 1707 तक वाराणसी की पहाड़ियाँ, विशेष रूप से दो उत्तरी पहाड़ियाँ, अपनी प्राकृतिक शांति को बनाए रखने में सफल रही थीं।
टेवरनियर ने बिंदुमाधव मंदिर का बहुत ही सजीव विवरण दिया है, क्योंकि इस मंदिर की भव्यता ने उसे चकित कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे मच्छोदरी के पास हिंदू मंदिरों के समूह के बीच स्थित अशोक स्तंभ ने उसे प्रभावित किया था। यह स्तंभ 1809 के सांप्रदायिक दंगों में नष्ट कर दिया गया था।
मुगल दरबार के पतन के दिनों में वाराणसी का प्रशासन लखनऊ के नवाबों के अधीन आ गया, जिन्होंने शिया समुदाय को संरक्षण दिया और इस कारण वे कम कट्टर थे।
नवाबों के अधीन, एक उदार शासक मीर रुस्तम अली ने वाराणसी में कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए होली के बाद बसंत के आगमन को चिह्नित करने के लिए "बुढ़वा मंगल" नामक उत्सव की शुरुआत की, जिसमें दोनों समुदाय सक्रिय रूप से भाग लेते थे।
मीर रुस्तम अली ने मन-मंदिर घाट के पास एक किला बनवाया था, जिसके खंडहर अब भी देखे जा सकते हैं। मीर घाट आज भी उनके नाम को संजोए हुए है।
वर्तमान रामनगर किला, जिसे राजा बलवंत सिंह ने बनवाया था, वास्तव में मीर रुस्तम अली के नष्ट किए गए किले की सामग्री से बनाया गया था।
यदि हम गंगा के किनारे वाराणसी के दक्षिणी भाग को देखें, विशेष रूप से पंचगंगा और मणिकर्णिका घाट के दक्षिण में, तो हमें स्वीकार करना होगा कि इस क्षेत्र के विकास में मीर रुस्तम अली का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था।
उनके अधिकारी मांसा राम और बलवंत सिंह, जिन्होंने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह (1719) से वाराणसी के राजा की उपाधि प्राप्त की, ने पहाड़ियों पर शहर को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आज जो वाराणसी हम देखते हैं, वह सुरम्य घाटों और सुंदर टेरसदार भवनों से सुसज्जित अर्धचंद्राकार नगर, मुख्य रूप से मराठों की देन है, जिनकी गतिविधियाँ 1712 में शुरू हुईं और 1795 में अपने चरम पर पहुँच गईं।
1734 और 1789 के बीच मराठों का वाराणसी में पूर्ण नियंत्रण था। इस दौरान उन्होंने मुगल दरबार पर अपना प्रभाव बनाए रखा।
1761 में पानीपत के युद्ध में हार के बाद, वे अपनी सैन्य शक्ति को पुनः स्थापित करने में असफल रहे और इसलिए उन्होंने वाराणसी, अयोध्या और प्रयाग (त्रिस्थली) को मुक्त कराने की योजना पर बल देना बंद कर दिया। हालाँकि, वे अब भी जनता के लिए छोटे-छोटे सार्वजनिक कार्यों में योगदान देते रहे।
इस अवधि के दौरान कई घाट, मठ और ब्रह्मपुरियाँ बनाई गईं:
● ब्रह्म घाट
● दुर्गा घाट
● त्रिलोचन घाट (नारायण दीक्षित के प्रयासों से निर्मित)
● मंगलागौरी घाट
● दलपत घाट
● बालाजी घाट
● अहिल्या बाई घाट
● राणा घाट
● मुंशी घाट (जो नागपुर दरबार के एजेंट मराठा मुंशी श्रीधर द्वारा निर्मित था)
1932 तक वाराणसी के अधिकांश घाट बन चुके थे। स्वतंत्र भारत की सरकार ने कुछ घाटों की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया, लेकिन नए घाट बनाने की दिशा में कोई बड़ा प्रयास नहीं किया गया।
नारायण दीक्षित एक विलक्षण व्यक्ति थे, जिनमें बुद्धिमत्ता और धार्मिकता, ज्ञान और सेवा का अद्भुत मेल था।
जब घाटों को पत्थरों से ढका गया और कुछ स्थानों पर 100 से अधिक सीढ़ियाँ बनाई गईं, तो उन्होंने महसूस किया कि गर्मियों में जलते हुए पत्थरों पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए चलना कठिन होगा। उन्होंने इसे "धार्मिक सेवा" के रूप में स्थापित किया कि गर्मियों के दौरान घाटों की सीढ़ियों को छप्परों से ढका जाए।
उन्होंने घाटों पर छायादार बाँस की छतरियाँ लगाने की परंपरा भी शुरू की, जो अब वाराणसी की एक विशिष्ट पहचान बन चुकी हैं।
वाराणसी के लोगों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के बाद, दैनिक श्रमिकों, कारीगरों और कलाकारों के परिवारों ने अपनी पारंपरिक आजीविका खो दी (जो मुख्य रूप से मंदिरों से जुड़ी थी, जो अब अस्तित्व में नहीं थे), और उनका अस्तित्व अस्थिर हो गया। उन्हें नए और सुरक्षित आवासों की तलाश करनी पड़ी, जहाँ वे आगे के उत्पीड़न से मुक्त रह सकें और बार-बार अपने धर्मांतरित होने की स्थिति की याद दिलाने से बच सकें। मराठों के प्रभुत्व के दौरान यह उनके जीवन का और भी संवेदनशील मुद्दा बन गया। उन्हें 'अछूत' और 'अशुद्ध' की श्रेणी में रखा गया, जिससे उनकी व्यक्तिगत गरिमा आहत हुई।
इस्लामी कानूनों ने सदियों से हिंदू जनता को सांस्कृतिक रूप से दबा रखा था, जो उनके लिए अत्यधिक अपमानजनक था (जैसे घुड़सवारी पर प्रतिबंध, पालकियों का उपयोग, या संगीतकारों के समूह के साथ जुलूस निकालने की मनाही आदि)। पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761) के बाद दिल्ली सरकार की शक्ति अत्यंत कमजोर हो गई। मराठों ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस नए हिंदू शासन के तहत वाराणसी की हिंदू आबादी ने श्रमिक वर्ग पर दबाव डालना शुरू किया, जिनमें से कुछ निश्चित रूप से इस्लामी धर्म के अनुयायी भी थे। धर्मांतरित लोगों को नए निवास स्थलों की तलाश करनी पड़ी, और उन्होंने मुख्य रूप से दशाश्वमेध बिंदु के उत्तर में पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानों को चुना।
पहाड़ियों की वास्तविक चोटियाँ 1761 तक निर्जन और जंगली बनी रहीं, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई और मराठों की हार हुई। इसने नाटोर की रानी भवानी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस विस्तृत निर्जन क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया और इसे बसाने का विचार किया। यह क्षेत्र, जो पहले डाकुओं और अपराधियों का अड्डा था, धीरे-धीरे एक सुसंस्कृत, कानून-पालन करने वाले ब्राह्मण विद्यालयों और छात्रावासों के क्षेत्र में बदल गया।
उन्होंने नदी के समानांतर एक गली (जो वास्तव में एक संकरी सड़क थी) का निर्माण करवाया और इसके दोनों ओर ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए। इस प्रकार बंगालीटोला विकसित हुआ, जो जल्द ही दक्षिण के जंगम संन्यासियों द्वारा विकसित जंगमबाड़ी से सटा हुआ था। जंगम संन्यासी प्रसिद्ध समाज सुधारक और दार्शनिक संत बसवा द्वारा स्थापित वीर-शैव समुदाय से संबंधित थे।
इस अद्वितीय कार्य के अलावा, रानी भवानी ने कई मंदिरों, अतिथिगृहों, अन्नक्षेत्रों और अपनी स्वयं की एक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, जिससे यह संपूर्ण क्षेत्र दान और सेवा का केंद्र बन गया। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर, पूर्व और पश्चिम बंगाल के कई अन्य जमींदारों ने भी मंदिरों के साथ अन्नक्षेत्र (सत्र) की स्थापना की।
भोजन की तलाश में गरीब लोग यहाँ एकत्र होने लगे। धीरे-धीरे यह गली लोकप्रिय हो गई, और दोनों ओर व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल दीं। समय के साथ, गलियों और संकरी बस्तियों का एक जाल बिछ गया, जहाँ हजारों लोग बसने लगे। विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए यह क्षेत्र अंतिम जीवन यात्रा की प्रतीक्षा करने के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया।
पूरा क्षेत्र पश्चिमी ढलानों से फैला हुआ था और ऐसे कुख्यात स्थानों की सीमा तक पहुँचा, जैसे केनाराम के जंगल, बटुक भैरव, बड़ा देव और लहुरिया बीर, जो सभी गणों के ठिकाने थे।
शहरीकरण तेजी से फैलने लगा। जो कभी वीरान जंगल था, वह जल्द ही पूरे भारत से आए लोगों से भर गया, जो इस विश्वास के साथ यहाँ आए थे कि जब वे मरेंगे, तो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जल्द ही, वाराणसी, जो पहले से ही शास्त्रीय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी, कश्मीर, मिथिला, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और बंगाल के प्रमुख विद्वानों का एक मिलन स्थल बन गई।
नदी और रेल परिवहन के विकास से इस स्वागतयोग्य प्रव्रजन को और बढ़ावा मिला।
यह स्पष्ट करता है कि गोधौलिया बिंदु से पश्चिम, दशाश्वमेध से पूर्व, असी से दक्षिण और सिगरा से दक्षिण-पश्चिम तक का क्षेत्र रानी भवानी (1756) और इंदौर की विधवा होल्कर रानी अहिल्या बाई (1766-95) से पहले अस्तित्व में नहीं था।
वाराणसी का दक्षिणी भाग वास्तव में इन दो विधवा महिलाओं की पहल का परिणाम था।
रानी भवानी और अहिल्या बाई से पहले और बाद की वाराणसी बिल्कुल अलग दिखती थी। उनके दान और योगदान की सूची बहुत लंबी है। अहिल्या बाई घाट और अहिल्या बाई ब्रह्मपुरी आज भी उनकी धार्मिक और परोपकारी प्रवृत्ति के स्थायी प्रमाण हैं।
उनका सबसे बड़ा और स्थायी उपहार विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण था, जिसे आज हम देखते हैं, जो मस्जिद के ठीक सामने स्थित है।
यह कोई आसान कार्य नहीं था। सदियों की अराजकता और ध्वंस के कारण इकट्ठे हुए कचरे और मलबे को हटाना और स्तंभों से युक्त एक नया मंडप और मंदिर परिसर बनाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था।
सदियों की लूट और विनाश के कारण पूरे मंदिर परिसर, निवास, उद्यान, मीनारें, गुंबद, स्तंभ – सब कुछ मलबे में बदल गया था।
इन अवशेषों को खोदकर अतीत को पुनः प्राप्त करना असंभव था, इसलिए इस ढेर को समतल कर एक सड़ी हुई झील को भर दिया गया। इससे एक चौड़ी सड़क, गलियाँ और एक खुला प्रांगण तैयार किया जा सका।
इस्लामिक मस्जिद की सीमाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गईं।
रानी भवानी और अहिल्या बाई ने अपमानित हिंदू समुदाय के सिर से एक अभिशाप हटा दिया।
नया मंदिर ज्ञानवापी के किनारे बनाया जाना था, और इसे उसके दक्षिणी तट पर स्थापित किया गया।
आज वही नया विश्वनाथ मंदिर रानी अहिल्या बाई होल्कर द्वारा निर्मित खड़ा है।
प्रसिद्ध अविमुक्तेश्वर को भी एक स्थान दिया गया और उन्हें मंदिर के दक्षिण-पूर्वी कोने में प्रतिष्ठित किया गया।
हालांकि यह मंदिर संकीर्ण था और मूल मंदिर की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन इसकी शोभा पंजाब के सिख महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दी गई स्वर्ण-आवरण से पुनः प्राप्त की गई।
इतिहास में इस निरंतर विध्वंस और पुनर्निर्माण के बावजूद, एक विशेष विवरण ने अब भी भक्तों को सांत्वना दी।
मूल पीपल का वृक्ष, जो ज्ञानवापी के दक्षिण-पश्चिमी कोने में स्थित था और जिसका उल्लेख काशी खंड में है, आलमगीर के शाही आदेशों की अवहेलना करते हुए फिर से अंकुरित हो गया।
जिस सड़क ने पुराने मंदिर को ज्ञानवापी से जोड़ा था, वह कचरे और मलबे से अवरुद्ध हो गई थी।
रानी भवानी ने गंगाद्वारि चैनल को काटकर एक नया मार्ग बनाया, जो आज विश्वनाथ गली के रूप में जाना जाता है।
इसने दो प्रसिद्ध यक्ष मंदिरों को भी पुनर्जीवित किया – डंडपाणि भैरव और धुंधिराज।
वाराणसी के इस नए विस्तार ने धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और दशाश्वमेध से असी तक हिंदू राजकुमारों ने घाटों का निर्माण कराया।
रानी भवानी ने कई पवित्र जलकुंडों का जीर्णोद्धार किया, जैसे:
● लोलार्क कुंड
● कुरुक्षेत्र कुंड
● दुर्गा कुंड (प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर सहित)
● पिशाचमोचन कुंड
● कपिलधारा
● सूर्य कुंड
● लहरियातालाब
● ईशरगंगी
उन्होंने पंचक्रोशी मार्ग (50 मील लंबा) पक्का करवाया और इसे वृक्षों और विश्राम गृहों से सजाया।
यह नई वाराणसी इन्हीं दो महान महिलाओं और भारत के विभिन्न राज्यों के अन्य हिंदू शासकों की देन है।
14.अंतिम प्रहार
I
हमने (1) वाराणसी के मूल नगर की पुनर्खोज करने, (2) उस अन्य विस्तार का लेखा-जोखा तैयार करने, जिसे इसी नाम से जाना जाता है, और (3) संयोगवश (a) उन परिवर्तनों पर ध्यान देने का प्रयास किया, जिन्हें वाराणसी को युगों तक झेलना पड़ा, तथा (b) उन विध्वंसों को समझने का प्रयास किया, जिन्हें बाहरी नगर-निर्माताओं ने जानबूझकर, न कि संयोगवश, अंजाम दिया।
इन परिवर्तनों को लागू करते समय, दुर्भाग्यवश उन्होंने केवल प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा, और नगर की प्राचीन ऐतिहासिकता, यदि उसकी पवित्रता नहीं तो भी, की परवाह नहीं की। यह संदेह होता है कि क्या वे इस पवित्र कार्य की विशालता को समझने के लिए पर्याप्त सक्षम थे, और उन्होंने जिस ऐतिहासिक कार्य को अंजाम दिया, उसमें उनकी अज्ञानता और भूल कितनी बड़ी थी।
जाटकों में उल्लिखित प्रसिद्ध स्थान वाराणसी, जहाँ गौतम बुद्ध ने अनेकों उपदेश दिए थे, संभवतः उस स्थान के निकट रहा होगा जिसे हम आज सारनाथ (सारंगनाथ) के रूप में जानते हैं, जहाँ मृगदाव (जिसे ईशिपत्तन भी कहा जाता था) में बुद्ध निवास करते थे। उनके निवास स्थान को सावधानीपूर्वक चुना गया होगा, क्योंकि एक उपदेशक के रूप में वे आसानी से श्रेष्ठियों (व्यापारियों) तक, साथ ही उन आम नागरिकों तक पहुँच सकते थे जो बाजारों में भीड़ लगाते थे।
अपने जीवन में वे इतने महान व्यक्ति थे कि समाज के दोनों वर्गों तक पहुँचने में सक्षम थे। और दोनों समुदायों ने उन्हें जीवन के एक असाधारण मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया।
सारनाथ-भाग के अतिरिक्त, एक व्यापारिक, प्रशासनिक और धार्मिक वाराणसी भी थी, जो प्रभावशाली व्यापारियों और ब्राह्मण पुरोहितों के वर्चस्व में थी।
सारनाथ केवल वाराणसी का एक आध्यात्मिक विस्तार रहा होगा, जिसे एक महत्वपूर्ण ब्राह्मणीय केंद्र माना जाता था।
महाश्मशान (गौरीपीठ/रुद्रवास) और आनंदकाननम के सुंदर आश्रम निश्चित रूप से उन क्षेत्रों से जुड़े उपयुक्त विशेषण थे जो इन विवरणों से मेल खाते थे।
हम पहले ही वाराणसी के भौगोलिक स्वरूप को वारणा और असी-नाले के बीच कई स्पष्ट रूप से परिभाषित खंडों में विभाजित कर चुके हैं।
पहला खंड वारणा के उत्तर में स्थित घाटी को संदर्भित करता है, जो कपिलधारा (कैथी) और भीतरी (लगभग 20 किमी दूर) तक फैली हुई थी।
लेकिन क्या इस खंड को आम तौर पर मान्यता प्राप्त वाराणसी की सीमाओं में शामिल करना प्रामाणिक है?
आइए इस पर विचार करें। हमारे पास हमारे दावे के समर्थन में महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हैं।
महाभारत वाराणसी का उल्लेख गंगा और गोमती के बीच स्थित एक नगर के रूप में करता है।
हमें दिवोदास की हर्यश्व पर विजय और 'एक नए नगर' की स्थापना का उल्लेख मिलता है, जिसे आगंतुक ने वाराणसी के रूप में नामित किया, यह पुरानी वाराणसी के लिए एक चुनौती थी। समय के साथ, इस नए नगर को शिव-गणों द्वारा नष्ट कर दिया गया, जो वाराणसी के नाम को एक राजसी उपहास में परिवर्तित होते नहीं देख सकते थे। (महाभारत: अनुशासन पर्व, 1899-1900)। हम मानते हैं कि वर्तमान वैनरथा इस प्रसिद्ध नगर की एक हल्की सी याद भर है।
● एक संकीर्ण जल-संपर्क कपिलधारा और वारणा को जोड़ता है, जो अंततः वैनरथा और गाजीपुर तक पहुँचता है। हालाँकि यह अब संकीर्ण और महत्वहीन प्रतीत होता है, यह संपर्क प्राचीन अवश्य ही रहा होगा।
● इसकी प्राचीनता इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि इस मार्ग के साथ प्राचीन कलाकृतियाँ और टेराकोटा की वस्तुएँ खोजी गई हैं। इससे भी महत्वपूर्ण, ब्राह्मी लिपि में मुद्राएँ और प्राचीन ईंटें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं।
● खुदाई अब भी जारी है और इससे बड़ी संभावनाएँ जुड़ी हुई हैं।
महाभारत के अलावा, कृत्यकल्पतरु भी एक दूसरी वाराणसी, दिवोदास की वाराणसी का उल्लेख करता है। यह अत्यधिक संभावना है कि यह आधुनिक वैनरथा ही हो।
यह बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह दिखाना आवश्यक है कि भूले-बिसरे नगर वैनरथा और भीतरी, साथ ही कैथी गाँव और वारणा नदी के बीच की भूमि वास्तव में एक शहरी बस्ती थी, जो एक संपन्न बाज़ार गतिविधियों से भरी थी। (इन क्षेत्रों की व्यक्तिगत यात्रा ने लेखक को इसके महान अतीत के प्रति आश्वस्त कर दिया।)
इस शहरी क्षेत्र के पश्चिम में सारनाथ के मठ स्थित थे, जहाँ मृगदाव, बुद्ध का विशेष निवास स्थान था। वे निश्चित रूप से अपने मठ को नगर के निकट रखना चाहते थे, जिससे वे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें।
यह प्रमाणित करता है कि बुद्ध किसी निर्जन स्थान पर उपदेश नहीं दे रहे थे। अत्यधिक संभावना है कि उन्होंने अपने उपदेश पहले से ही बसे-बसाए स्थानों पर दिए होंगे। इस भौगोलिक क्षेत्र में प्राचीन समय में एक संपन्न आबादी अवश्य रही होगी।
तो प्रश्न उठता है, इस क्षेत्र को नष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार था? निश्चित रूप से कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं। यह क्षेत्र इस्लामी आक्रमण से बहुत पहले ही उजाड़ दिया गया था। (यही कारण है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सारनाथ पर कभी हमला नहीं किया)।
दूसरा खंड नगर के किले वाले क्षेत्र से संबंधित है, जो स्पष्ट रूप से वारणा-संगम के पास स्थित था।
● यहाँ मच्छोदरी-नाला निकट ही बहता था। इस नाले के मोड़ पर एक प्राचीन मिट्टी का किला स्थित था, जिसे भारा-शिव कबीले ने बनाया था।
● वाराणसी का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र उस झील के चारों ओर विकसित हुआ, जहाँ जलमार्गीय व्यापार को एक सुरक्षित बंदरगाह प्राप्त था।
● तब से, सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान इसी क्षेत्र में स्थित रहे हैं, जिसे पक्की महल के रूप में जाना जाता है।
● यह क्षेत्र जतनबर, काल भैरव, चौखंभा, मंगलागौरी, ठठेरी बाजार, असि भैरव, त्रिलोचन, कुँजीटोला, लक्ष्मी चौबुत्रा आदि को समेटे हुए है।
काशी खंड में इस पूरे क्षेत्र को, उसके प्रतिष्ठित मंदिरों (त्रिलोचन, बिंदुमाधव, ओंकार, कृतिवास, महाकाल, अविमुक्त) के साथ अंतरगृह के रूप में चिन्हित किया गया है।
आज इनमें से अधिकतर मंदिर खंडहर बन चुके हैं; कुछ मस्जिदों में परिवर्तित कर दिए गए।
तीसरा खंड मांडाकिनी झील और उसके परिवेश से संबंधित है।
● यह झील विशाल और प्राकृतिक रूप से इतनी सुंदर थी कि प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार जेम्स प्रिंसेप ने इसके कई चित्र बनाए थे।
● झील के किनारे बड़ा गणेश मंदिर था, जो प्राचीन गण संप्रदाय की महत्ता का प्रमाण था।
● इस झील के आसपास के जंगल और दलदली क्षेत्र उपनगर के रूप में जाने जाते थे, जहाँ अमीर लोग अपने बगीचे-बंगले बनवाते थे।
● यह झील गंगा से मच्छोदरी चैनल के माध्यम से जुड़ी थी, जिससे जहाजों की आवाजाही होती थी।
आज इस झील के केवल दो दुखद अवशेष बचे हैं:
1. कंपनी गार्डन का तालाब
2. बुलानाला कुंड, जो अब एक बदबूदार, गंदे पानी का दलदल बन चुका है।
इस्लामी दृष्टिकोण, जैसा कि बाबर की आत्मकथा से स्पष्ट होता है, प्रकृति की सुंदरता और उसके संरक्षण को प्रोत्साहित करता था। स्वच्छता और सजावट तथा सौंदर्य की वस्तुओं की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था इस्लामी मानस का एक अभिन्न अंग थी। मुसलमानों ने वाराणसी के मनोरम सौंदर्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यदि ऐसा है, तो फिर प्रार्थना करें कि वाराणसी की झीलों और जलधाराओं के अतिक्रमण के लिए कौन उत्तरदायी था? किसने इस महान नगर और उसके परिवेश के अद्वितीय चरित्र को स्थायी रूप से नष्ट कर दिया?
झील का विनाश, जो वास्तव में एक विनाशकारी दुर्भाग्य था, मात्र मंदिरों और मूर्तियों के विध्वंस से किसी भी प्रकार कम पापपूर्ण नहीं था। इतिहास उत्तरार्ध को उजागर करता है, लेकिन पूर्व के बारे में पूरी तरह मौन है। वास्तव में, इतनी विशाल ठंडे दिमाग से की गई बर्बरता, जिसने जनता की कोमल भावनाओं के प्रति स्पष्ट उपेक्षा दिखाई, सौंदर्यपरक नगर-निर्माताओं और विवेकी नागरिकों से कड़ी निंदा की पात्र है।
जनभावनाओं के संगठित उल्लंघन ने ब्रिटिश शासन के अत्यधिक व्यावहारिक प्रशासनिक शैली को चिह्नित किया, जिसे पूरी तरह एक व्यापारिक दृष्टिकोण से संचालित किया गया था। कोई भी चीज़, जो दूर से भी ब्रिटिश जीवनशैली से भिन्न थी, संकीर्ण व्यापारी समुदाय की ओर से बहुत कम सहानुभूति प्राप्त कर पाई।
लोगों के अधिकारों के बार-बार उल्लंघन ने इंग्लैंड की संसद को ऐसे दंभी अधिकारियों जैसे कि क्लाइव और हेस्टिंग्स के कुकर्मों की कड़ी समीक्षा करने के लिए मजबूर किया। उन्हें ठीक ही अभियुक्त ठहराया गया और निंदा की गई। लेकिन एक और बाद का, और अधिक निंदनीय भारतीय जीवन के विनाशकारी शासक डलहौज़ी, जो इंग्लैंड के कुलीन वर्ग से था, पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया। यह वही डलहौज़ी था, जिसकी साम्राज्यवादी नीति ने 1857 के महान विद्रोह को जन्म दिया। संभवतः, उसे इसलिए बख्श दिया गया क्योंकि वह अपने समय के उच्च सामाजिक वर्गों में प्रभावशाली था।
नहीं, 1857 के कठोर पाठ से पहले भारत में ब्रिटिश शासन की तस्वीर एक उदास करने वाली थी, जिसमें शासन करने वाले सख्त अनुशासनप्रिय और आत्मसंतुष्ट थे, जो हमेशा देश के ‘स्थानीय निवासियों’ के प्रति एक स्पष्ट श्रेष्ठता की भावना रखते थे, जिन्हें समझने की उन्होंने कभी परवाह नहीं की।
वाराणसी से संबंधित एक ऐसे ही घटना का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो पूरी तरह से ब्रिटिश कुप्रशासन द्वारा भड़काई गई थी। यह घटना 1795 में हुई थी और 1809 तक पूरी तरह से नियंत्रित की जा सकी। वाराणसी के नागरिक जीवन को एक महत्वपूर्ण उथल-पुथल ने हिला दिया, जो अब तक विदेशी शासकों की मनमानी कार्यशैली को सहन नहीं कर पा रहा था।
वाराणसी के वीरशैव और अघोरी परंपराओं के अनुयायियों ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को संजोकर रखा, जिसने उन्हें किसी भी ऐसे कार्य के विरुद्ध विरोध करने के लिए प्रेरित किया जिसे उन्होंने अपने अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा। उनके व्यवहार में एक प्रकार की निराशा की भावना स्पष्ट थी। इस प्रकार, वे एकजुट हुए और खुलकर विरोध में आ गए।
ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐसा स्वतः स्फूर्त और जन-समर्थित प्रदर्शन 1857 तक फिर कभी नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से, यह विस्फोट शासकों के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। यह था वाराणसी का जवाब वॉरेन हेस्टिंग्स की तानाशाही नीति के विरुद्ध।
ब्रिटिश शासन के कारण वाराणसी की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो गई थी, जिसका मुख्य कारण स्थानीय जनता के सम्मान और पारंपरिक अधिकारों को ठेस पहुँचाना था। वे अपने सम्मान को कलंकित महसूस कर रहे थे और उनकी महिलाओं का अपमान हुआ था। वे स्वयं को सामाजिक भारत में अपने वैध स्थान से वंचित समझने लगे थे।
उन घटनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिन्होंने उन्हें तत्काल भड़काया:
(a) अवध के नवाब को पदच्युत किया जाना,
(b) उनका जबरन और निरंकुश निर्वासन कोलकाता में,
(c) अवध की बेगमों का अपमान, और
(d) बनारस के राजा के साथ किए गए क्रूर और अविनयपूर्ण व्यवहार। यह राजा प्रतीकात्मक रूप से हिंदू भारत के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता था।
उस समय की सामंती उत्पीड़नों के बावजूद, लोगों ने अपनी पहचान और गौरव को पारंपरिक शासक घरानों से जोड़ा। नवाब मुस्लिम थे, और राजा हिंदू था। लेकिन उनके लिए यह भेद कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उन्होंने ‘फिरंगियों’ (जैसा कि यूरोपियों को कहा जाता था) के हस्तक्षेप को सभी समुदायों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने विदेशियों को हड़पने वाले (अधिकार छीनने वाले) के रूप में देखा और कभी भी उनके शासन को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया, सिवाय बलपूर्वक। शांत जनता भीतर ही भीतर उबल रही थी।
जब उनके शासकों और उनकी महिलाओं का अपमान किया गया, तो जनता बुरी तरह क्रोधित हो गई। एक गहरी असंतोष की भावना वातावरण में व्याप्त हो गई।
जल्द ही, लोगों ने एक विदेशी व्यापारिक समुदाय के शाही परिवारों के मामलों में हस्तक्षेप के प्रति अपने आक्रोश को प्रदर्शित किया।
"किन्हीं व्यापारियों के एक समूह को यह अधिकार किसने दिया?" उन्होंने तर्क दिया, "कि वे व्यापार के नाम पर भारत में प्रवेश करें, फिर राजाओं के साथ दुर्व्यवहार करें और एक स्थापित सरकार को अस्थिर कर दें?"
पहला विरोध वज़ीर अली (1795) के नेतृत्व में हुआ, जो अवध के असफ-उद-दौला के पुत्र थे। यह एक जनविद्रोह था, जिसमें सभी समुदायों ने भाग लिया।
लेकिन जल्द ही इस विद्रोह की दिशा एक सांप्रदायिक संघर्ष (1809) से भटक गई, जिसमें भारी रक्तपात हुआ। इसी संघर्ष के दौरान, लाट भैरव और मच्छोदरी के बीच खड़ा महान स्तंभ (अशोक स्तंभ?) तोड़ दिया गया।
हम इन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उस समय की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को, चाहे अल्प रूप में ही सही, इंगित करती हैं। ये तत्कालीन सत्ताधारी शक्ति के निरंकुश आचरण को उजागर करती हैं।
वाराणसी का विनाश भी उसी प्रकार के एक असंवेदनशील रवैये का परिणाम था, जिसमें उन लोगों के सामाजिक मूल्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं था, जिन्हें वे 'देशी' कहकर उपहास करते थे।
यह विद्रोह इतना गंभीर था कि ब्रिटिश एजेंट पर हमला हुआ, और वह केवल एक चतुर युक्ति के कारण बाल-बाल बचा। इस योजना में कुछ महिलाओं और एक 'देशी' व्यापारी ने सहायता की। कई अंग्रेज मारे गए, जिनमें रेजिडेंट के सहायक-ए-कैंप भी शामिल थे।
इस अत्यधिक भयावह स्थिति में, विदेशी शासक वर्ग को अमीर नागरिकों द्वारा प्रदान किए गए उद्यान-गृहों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये घर, जैसा कि हम जानते हैं, संकट के केंद्र से बहुत दूर सुरक्षित स्थानों पर स्थित थे।
अंग्रेज़ी अभिलेखों में हमें उनके इन सुरक्षित आश्रयों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें वे "शहर क्षेत्र से बाहर", "निर्जन भागों में" बताते हैं, जो कि संपन्न व्यापारिक वर्ग की संपत्तियाँ थीं।
इन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि कबीरचौरा और नदेसर (जिसमें जगतगंज, नाटे इमली और वरुणा पुल क्षेत्र शामिल था) के बीच कई बाग-बग़ीचे और उद्यान-गृह थे।
सामान्य रूप से, वाराणसी का यह भाग कभी हरे-भरे और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था, जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है।
उपरोक्त तथ्यों के गहन अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि झील का उत्तर-पश्चिमी भाग उस समय "शहर का उपनगर" माना जाता था, और शहर की सीमाएँ मांडाकिनी तालाब के दक्षिणी किनारों पर समाप्त होती थीं।
प्राचीन नगर के प्रारूप को समझने में ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि मुख्य नगर धीरे-धीरे अपने उत्तरी केंद्र से दक्षिण की ओर विस्तार कर रहा था, और यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक जारी रही। जो आज हम देखते और सराहते हैं, वह एक प्राचीन नगर का विस्तार मात्र है, जिसका एक भाग विलुप्त हो गया, और दूसरा शहर की सीमाओं से बाहर धकेल दिया गया।
ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन वाराणसी का केवल एक छोटा सा अंश ही अपनी मूल केंद्रीय पहचान से अब भी जुड़ा हुआ है।
वाराणसी की आत्मा को हमेशा के लिए उड़ान भरने के लिए विवश कर दिया गया, उन लोगों की कृपा से जो यह समझने में असफल रहे कि वाराणसी हिंदू मानसिकता के लिए क्या महत्व रखती है।
इस तीसरे खंड को, यहाँ तक कि इस्लामी शासनकाल के दौरान भी, नगर की सीमा माना जाता था—यानी नगरीकृत वाराणसी का अंतिम छोर।
नगर क्षेत्र की सीमाएँ वरुणा नदी द्वारा निर्धारित की गई थीं। मांडाकिनी झील, उसके आस-पास का क्षेत्र, मच्छोदरी झील और नाला, यहाँ की सघनतम आबादी को आश्रय प्रदान करते थे। कई महत्वपूर्ण मंदिरों की उपस्थिति ने इस क्षेत्र को और भी महत्वपूर्ण बना दिया।
इस क्षेत्र के आगे वाराणसी का स्वरूप अपेक्षाकृत शांत था, जहाँ 1840 तक हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य फलता-फूलता था।
वास्तविकता यह है कि, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया, शहर एक कंकरीली पहाड़ी श्रृंखला के ऊपर स्थित था, जो नदी की ओर ढलान बनाती थी और फिर उससे आगे तक फैली हुई थी। गंगा नदी अपने स्वयं के तल पर प्रवाहित होती थी, लेकिन उसके तल के नीचे और भी बड़ी जलधारा बहती थी।
कई झीलें और जलधाराएँ पश्चिमी ढलानों से जल एकत्र करती थीं, और कंकरीली परतों के माध्यम से रिसकर नदी को पोषित करती थीं। वर्षों से यह देखा गया कि जब नदी में बाढ़ आती थी, तो प्राचीन वाराणसी की सभी झीलों, तालाबों और जलधाराओं का जलस्तर स्वतः ही बढ़ जाता था।
इन झीलों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं—अगस्त्यकुंड, लक्ष्मीकुंड (जिसे मिसिर पोखरा भी कहा जाता था), और विशाल बड़ियातालाब। इसके अतिरिक्त, पिशाचमोचन और सूरजकुंड को भी इसमें जोड़ा जा सकता है।
ईशरगंगी कभी एक और बड़ा तालाब था, जो गंगा के जलस्तर के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होता था। कुरुक्षेत्र और लोलार्क भी गंगा के साथ जुड़े हुए थे।
बड़ियातालाब, मिसिर पोखरा, लक्ष्मीकुंड, सूरजकुंड, पिशाचमोचन, लोलार्क, कुरुक्षेत्र और रेवती तालाब निश्चित रूप से उस समय नगर-सीमा के "बाहरी" क्षेत्र माने जाते थे। यदि इस तथ्य का कोई प्रमाण आवश्यक है, तो हम औरंगाबाद चौकी और लक्सा चौकी के अस्तित्व का उल्लेख कर सकते हैं। ये शहर की चुंगी चौकियाँ थीं, जो नगर की सीमाओं को इंगित करती थीं। ये अभी भी कार्यरत हैं (1991)।
चौथा खंड विश्वनाथ पर्वत के चारों ओर स्थित था। यह क्षेत्र सबसे अधिक सघन बसा हुआ था, क्योंकि सभी लोग व्यापारिक केंद्र के निकट रहना चाहते थे। महान मंदिर की निकटता एक अतिरिक्त आकर्षण थी।
वरुणा और मच्छोदरी के किनारे के बड़े मंदिरों के विध्वंस के बाद, वाराणसी में अपेक्षाकृत कम महत्व रखने वाले विश्वनाथ मंदिर को नगर का सबसे महत्वपूर्ण देवालय माना जाने लगा।
इस प्रकार, उत्तर में मांडाकिनी झील और बुलानाला से लेकर दक्षिण में विश्वनाथ मंदिर, गोदौलिया और दशाश्वमेध तक, पूर्व में गंगा और पश्चिम में लक्ष्मीकुंड तथा रेवतीकुंड (रेओरितालाब) तक, वाराणसी का यह चौथा और सबसे व्यस्त क्षेत्र युगों से बिना किसी बाधा के फलता-फूलता रहा।
एकमात्र अंतर यह था कि नगर के आकर्षण का केंद्र अब वरुणा के पारंपरिक मोर्चे की ओर न होकर विश्वनाथ पर्वत की ओर था। वरुणा की महत्ता बड़े पैमाने पर मंदिरों के विध्वंस के कारण कम हो गई थी।
इस क्षेत्र की समृद्धि का अर्थ वाराणसी की समृद्धि था। इस क्षेत्र में शांति का अर्थ वाराणसी की शांति था। यहाँ अशांति और रक्तपात का अर्थ वाराणसी में अशांति और रक्तपात था।
इस क्षेत्र से आगे, गंगा के किनारे, दशाश्वमेध से केदार तक फैली वह लंबी पर्वत-शृंखला थी, जिसका अक्सर उल्लेख किया जाता है।
यह एक विस्तृत इलाका था, जो नगर के व्यस्ततम पर्वतीय क्षेत्र से आगे फैला हुआ था। मराठों और राजपूतों के हस्तक्षेप से पहले, इस भाग को उपनिवेश बनाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ कोई महत्वपूर्ण तीर्थस्थल नहीं था।
इस परित्यक्त पहाड़ी क्षेत्र में जीवन का संचार करने का श्रेय हिंदू भारत के राजघरानों को जाता है। वे इस्लामी शासकों को यह विश्वास दिलाने में लगे रहे कि इस पवित्र नगर का पुनर्निर्माण कर वे अपने शासन को भी गौरवान्वित करेंगे।
इस प्रकार, वाराणसी का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक गाथा बन गया।
वाराणसी के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र और इसकी पश्चिमी घाटी, रेओरितालाब (रेवतीकुंड) तक के विकास के लिए इतिहास दो महान विधवा-राजमाताओं (1) अहल्या बाई होल्कर, इंदौर और (2) रानी भवानी, नाटोर, बंगाल का ऋणी है।
हम पहले ही दोनों का उल्लेख कर चुके हैं। आज जो वाराणसी है, वह इन महिलाओं की उदारता के कारण ही है। उन्होंने इस तथ्य को सराहा कि वाराणसी का गौरव हिंदू चेतना का गौरव है। दोनों महिलाओं ने एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु पहल करते हुए एक नए वाराणसी को विकसित करने और पुराने को अलंकृत करने का कार्य किया। इनके महान प्रयासों से हिंदू संस्कृति को लाभ हुआ।
अब प्रश्न उठता है कि किसने महान झील और इसके जल से घिरे प्रसिद्ध वन क्षेत्र को पूरी तरह से मिट्टी में दफन कर दिया? वास्तव में किसने? मच्छोदरी चैनल का क्या हुआ? प्रसिद्ध नदियाँ—मांडाकिनी और गोदावरी—जिनका उल्लेख काशी खंड, काशी महात्म्य, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कृत्य कल्पतरु आदि में मिलता है, वे कहाँ और कैसे गायब हो गईं? किसने इन्हें नष्ट किया, और इन्हें नष्ट कर आनंदकानन की आत्मा को ही समाप्त कर दिया?
इन जल स्रोतों के अकारण विनाश ने वाराणसी के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। किसने या क्या कारण था इस प्रकार की बर्बरता का?
किसकी अज्ञानता, द्वेष, अथवा घोर उपेक्षा, जो कि एक विशाल अपराध के समान थी, इस संपूर्ण आपदा के लिए उत्तरदायी थी?
हिंदू-बौद्ध, जैन-बौद्ध संघर्षों ने सारनाथ की पवित्रता और एकांतता को नष्ट कर दिया माना जाता है। इस्लामी आक्रमणों ने मंदिरों को ध्वस्त किया और आंशिक रूप से लोगों को धर्मांतरित किया। लेकिन न तो एक ने और न ही दूसरे ने इस पहाड़ी नगर की प्राकृतिक संपदा—झीलों, तालाबों और नदियों को छुआ।
आज इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता। गोदावरी के निकट अगस्त्येश्वर मंदिर एक सुंदर पहाड़ी पर स्थित था (काशी खंड)। इसके तल में एक स्वच्छ झील हुआ करती थी। आज भी अगस्त्यकुंड के नाम से एक क्षेत्र इस विशाल जलाशय की स्मृति दिलाता है। लेकिन वास्तव में अब वहाँ कोई कुंड नहीं है। इसके स्थान पर नगर का सबसे बड़ा कूड़ा घर फल-फूल रहा है, जो हवा में भारी दुर्गंध घोल रहा है।
इसी प्रकार न तो भुतेश्वर तालाब है, न रुद्रसरोवर और न ही मणिकर्णिका कुंड। किसने इन्हें नष्ट किया? कैसे? क्यों? काशी खंड में जिन स्थलों का इतना गौरवपूर्ण वर्णन है, वहाँ सार्वजनिक शौचालय और कूड़ा घर क्यों बनाए गए? और किसने इस पवित्र स्थल पर एक अजीबोगरीब एंग्लिकन चर्च की रूपरेखा खड़ी कर इस प्राकृतिक विरासत को पूरी तरह से नष्ट करने का कार्य किया?
ये प्रश्न अत्यंत गंभीर हैं और इनका उत्तर दिया जाना चाहिए।
II
इतिहास लेखन की एक दुखद प्रवृत्ति यह होती है कि वह किसी न किसी साम्प्रदायिक या राजनीतिक कारण को प्राथमिकता देता है। जब इतिहास ऐसा करता है, तो वह इतिहास रह ही नहीं जाता। वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ इतिहास तैयार करना कठिन कार्य है। जब तथाकथित 'प्रगतिशील' मानसिकता वाले लोग वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं, तो दुःख होता है कि वे भी किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रचार में लिप्त हो जाते हैं।
कुछ इतिहासकारों के लिए यह आसान हो गया है कि वे इस्लामी जोश को धर्म के नाम पर की गई लूट और विनाश के लिए दोषी ठहराएँ। इस लोकप्रिय और सरल दृष्टिकोण को अपनाने से कई अन्य तथ्यों की अनदेखी हो जाती है। यह याद रखना लाभदायक होगा कि ऐसी भ्रांतियाँ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह और गलत व्याख्याओं की कुटिल चालों के कारण उत्पन्न होती हैं। समाजिक चेतना में योजनाबद्ध रूप से विष घोल दिया जाता है, और मानव मन पूर्वाग्रहों में अंधा हो जाता है।
इस बीच इतिहास पीड़ित होता है। वाराणसी इसका एक उदाहरण है। जहाँ इतिहास (क्या वास्तव में इतिहास?) मंदिरों के विध्वंस, लूट और अत्याचारों की आलोचना करता है, वहीं यह पवित्र तालाबों और धाराओं के विनाश और उनके उन्मूलन पर चुप्पी साधे रहता है।
यह अनायास नहीं हुआ। अगस्त्य, अत्रि, साम्ब, गौतम, भारद्वाज और अन्य कम प्रसिद्ध संतों और आचार्यों के आश्रम इन जलाशयों और धाराओं के किनारे बसे थे। दशाश्वमेध के पास ब्रह्मसरवर, रेवतीकुंड के पास रुद्रवासा, बटुकनाथ, बेलघरिया (बाद में केनाराम-स्थान के नाम से प्रसिद्ध), और बड़ियाबाग झील के पास स्थित आश्रम प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थे।
वाराणसी ने अपनी विद्या और आध्यात्मिक प्रयासों के लिए ख्याति प्राप्त की थी। मंदिरों या मूर्तिपूजा की संस्कृति के उदय से पहले भी (प्रथम से तृतीय शताब्दी तक) इसकी प्रसिद्धि इन्हीं संस्थानों पर टिकी थी।
इन प्राकृतिक और प्राचीन स्थलों का विनाश किसी भी प्रकार से मनुष्यों द्वारा निर्मित भवनों के विध्वंस से कम हानिकारक नहीं था।
वाराणसी के नागरिकों ने दो सौ वर्षों से अधिक समय तक अपनी प्राचीन धरोहरों के व्यवस्थित विनाश को सहन किया है। दूर के वे लोग, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पारंपरिक जीवन से पूर्णतः अपरिचित थे, उन्होंने बिना किसी संकोच के इस नगर की ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दिया, जिस पर उन्हें गर्व होना चाहिए था। वाराणसी को सदियों से अद्वितीय नगर माना जाता रहा है।
[लेखक ने स्वयं इन उथल-पुथल भरे समयों में मौन दर्शकों की खाली और असहाय निगाहों को देखा था। एक संपूर्ण जनसंख्या को निरंकुश दमन द्वारा सम्मोहित किया जा सकता है। ये वे दिन थे जब असी के राम मंदिर आंदोलन और जलियांवाला बाग जैसे भयावह घटनाएँ घटित हो रही थीं।]
यह भी देखा गया है कि अधिकांश नागरिक मंदिर विध्वंस के तथ्य से ही विचलित हो जाते हैं। हमने देखा है कि इस प्रकार की घटनाएँ अधिकतर तब घटित होती हैं जब मंदिरों में अपार संपत्ति संचित कर ली जाती है और उसे सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
यह प्रवृत्ति आज भी देखी जा सकती है। दक्कन, गुजरात और राजस्थान के बड़े मंदिर समय-समय पर अपने संचित धन को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखते हैं, जिससे संभवतः भक्तों को प्रेरित कर समान रूप से कीमती भेंट अर्पित करने के लिए उकसाया जाता है।
मंदिर विध्वंस का दोष केवल कुछ अत्याचारी शासकों पर लगाया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण आठ सौ वर्षों के इस्लामी शासन के दौरान अधिकांश प्रशासन ने हिंदू मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान किया। यदि हिंदुओं को वह कर देना पड़ता था जो इस्लामी धर्मशास्त्र कुरान के अनुसार गैर-मुसलमानों पर लगाया जाता था, तो उसी प्रशासन ने मुस्लिमों से भी ज़कात वसूली, जिससे हिंदू मुक्त थे।
यह मज़ेदार किंतु महत्वपूर्ण तथ्य है कि ब्राह्मणों ने शासकों से अपने लिए जज़िया कर से छूट प्राप्त कर ली थी।
इतिहास बार-बार कुछ चुनिंदा शासकों के कार्यों की चर्चा करता है, लेकिन उन अनेक शासकों के प्रशासनिक कौशल और सैन्य शक्ति की अनदेखी करता है, जिनकी सत्ता हिंदू समाज की भागीदारी पर निर्भर थी। व्यापार, कृषि और बैंकिंग जैसे क्षेत्र लगभग पूरी तरह से हिंदुओं के अधीन थे।
हिंदू समाज जबरन धर्मांतरण की समस्या को लेकर प्रतिक्रिया स्वरूप एक मानसिकता विकसित करने को उचित समझता है। यह एक गंभीर भूल है। इस पूर्वाग्रह ने राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुँचाया है। इससे समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग से स्थायी रूप से अलग-थलग हो गया है, जो पूरी तरह से तर्कहीन है। न तो तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं, न ही प्रगति इसे प्रोत्साहित करती है।
इतिहास बताता है कि जबरन धर्मांतरण के मामले वास्तव में नगण्य थे। जिन लोगों को उनके समुदाय ने अपवित्र और अछूत घोषित कर दिया, वे अनिवार्य रूप से किसी नए धर्म में चले गए। इन पीड़ितों को 'धर्मांतरित' कहना सत्य का उपहास करना होगा।
इसी प्रकार, दैनिक मजदूर, वेतनभोगी कर्मचारी, कारीगर, देवदासियाँ, वेश्याएँ, संगीतकार और पहले से ही बहिष्कृत अछूतों के मामले अलग थे। उन्होंने उस धर्म में अधिक सुरक्षा और कुछ 'सम्मान' पाया, जो सिद्धांततः मस्जिदों में समानता का पालन करता था और जातिगत भेदभाव को स्वीकार नहीं करता था।
इस्लामी समाज में गुलाम भी राजा और सम्राट बन सकते थे।
कुछ समुदाय, जैसे नाथपंथी, जैन और यहाँ तक कि बौद्ध भी, जिन्हें हिंदू समाज ने अपनाने से इंकार कर दिया था, उन्होंने सत्तारूढ़ धर्म को अपनाने में सुरक्षा देखी।
अंततः, हिंदू समाज के भीतर जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की समस्या ने उसे धर्मांतरण की समस्या से अधिक नुकसान पहुँचाया है।
वाराणसी में जबरन धर्मांतरण के मामले अपेक्षाकृत कम प्रतीत होते हैं। वास्तव में, वे लोग जिन्हें उनके ही भाइयों ने 'अपवित्र और सदा के लिए दूषित' घोषित कर दिया था, उनके लिए वापस लौटने के द्वार बंद हो गए थे।
हम वाराणसी के मंदिरों के विनाश की चर्चा करते हैं, लेकिन सारनाथ के विध्वंस और वाराणसी के गंगा-गोमती क्षेत्र के पूर्ण विनाश के बारे में चर्चा नहीं करते।
इतिहास में ऐसे मामले भी दर्ज हैं, जब हिंदू शासकों ने भी धार्मिक कारणों से अमानवीय कार्य किए।
आज, वाराणसी अपनी विशिष्टता खो चुकी है। यह अब केवल उत्तर प्रदेश का एक और नगर बन चुका है, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या गोरखपुर।
जिस दिन वाराणसी के प्राचीन वनों की हरियाली समाप्त कर दी गई, उसी दिन यह नगर अपनी गरिमा खो बैठा। इसे जबरन आधुनिकता की ओर धकेला गया और इसकी पवित्रता नष्ट कर दी गई।
आज का वाराणसी मात्र एक पर्यटन स्थल बनकर रह गया है। आधुनिक शहर-निर्माताओं की कठोर नीतियों ने इसे पत्थरों के शहर में बदल दिया, लेकिन इसके पीछे छिपी त्रासदी को बहुत कम लोग समझते हैं।
वाराणसी को देवताओं ने बनाया था, प्रकृति ने इसे अलंकृत किया था, और समय ने इसे स्वर्ग के समकक्ष स्थान दिया था।
लेकिन जब आधुनिक 'निर्माताओं' ने अपने बुलडोज़र और हथौड़े चलाए, तो यह विशेष स्थान सदा के लिए नष्ट हो गया। अब गंगा भी प्रदूषण की शिकार हो चुकी है।
आज न कोई मंदिर, न कोई मस्जिद, न कोई मठ, बल्कि पूरे वाराणसी की आत्मा को कुछ दशकों में बेरहमी से कुचल दिया गया।
वाराणसी के महान आत्मिक भाव को इस बदलाव ने स्वीकार कर लिया, यह समझे बिना कि वह वास्तव में क्या खो चुका है।
III
वास्तव में, इस मामले में जनता की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। वे केवल मूकदर्शक बने रहे और जो हो रहा था उसे चुपचाप सहते रहे। कुछ लोगों ने इन परिवर्तनों को सुधार के रूप में भी स्वीकार कर लिया।
आनंदकाननम परिसर को सबसे अधिक क्षति दो रेलवे स्टेशनों, राजघाट और कैंटोनमेंट, के निर्माण से हुई। तीसरा रेलवे स्टेशन, अलाईपुरा (बनारस सिटी), जो बाद में बनाया गया, उसने भी कई महत्वपूर्ण स्थलों को नष्ट कर दिया, जिनमें तीर्थ केंद्र बर्करिकुंड, सारनाथ क्षेत्र और वरुणा घाटी शामिल थे।
राजघाट या काशी रेलवे स्टेशन को उन लिमिटेड कंपनियों में से एक ने बनाया था, जो इंग्लैंड में पंजीकृत थीं और जिन्हें एक उपनिवेश के रूप में भारत को शोषण करने का पट्टा मिला था।
चूँकि ये कंपनियाँ केवल लालच और मुनाफे के लिए संचालित होती थीं, इसलिए उन्हें स्थानीय जनता की भावनाओं, उनकी संस्कृति या उनके धार्मिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं थी। इनके मालिक, शेयरधारक और ठेकेदारों के प्रमुख न तो इन मूल्यों से परिचित थे और न ही उन्हें किसी प्रकार की आत्मग्लानि थी। वे केवल अपने स्वामियों को संतुष्ट करने में लगे रहते थे।
अठारहवीं शताब्दी के अंग्रेजी समाज में विदेशी निवेश से होने वाले लाभों के प्रति अत्यधिक लालच भरा माहौल था। साउथ-सी बबल घोटाला इस तरह की वित्तीय लापरवाहियों का एक ज्वलंत उदाहरण है। दास व्यापार से हुए मुनाफे ने अठारहवीं शताब्दी में भयंकर वित्तीय संकट को जन्म दिया, जिसे संसद द्वारा चालाक बहसकर्ता विल्बरफोर्स के हस्तक्षेप से टाला गया।
ऐसे लालची माहौल में किसी भी सभ्यता के संरक्षण की अपेक्षा करना व्यर्थ था। किसी भी अंग्रेजी कंपनी को उस समय स्थानीय सांस्कृतिक धरोहरों या ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में दिलचस्पी नहीं थी, विशेष रूप से तब जब वे 'भूरे लोगों' से संबंधित थीं। कौन अजटेक, टॉलटेक, इंका और माया सभ्यताओं की प्राचीनता को बचाने की चिंता करता था?
शहर नियोजन जैसे व्यावहारिक और सौंदर्यपरक विषय को भी भावनात्मक मूल्यों, वास्तुकला संबंधी विचारों या पुरातात्विक आवश्यकताओं की अनदेखी कर क्रूरता से लागू किया गया। जो लोग इन कार्यों में लगे थे, उनमें कर्ज़न या प्रिंसेप जैसी ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। (या शायद, वे केवल न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने में लगे थे, ताकि अधिक धन लंदन की सजावट या टेम्स नदी पर एक और पुल बनाने में लगाया जा सके।)
रेलवे, सड़क निर्माण और शहरीकरण से जुड़े इन विदेशी इंजीनियरों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी मनमानी की। उनके एकमात्र उद्देश्य अपने निवेश पर लाभ बढ़ाना था। चूँकि उन्हें एक विदेशी प्रशासन और कठोर नौकरशाही का समर्थन प्राप्त था, इसलिए वे अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल रहे।
लॉर्ड कर्ज़न (1899-1905) के समय तक और सर विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेप जैसे विद्वान नौकरशाहों के हस्तक्षेप से पहले तक, प्राचीन स्मारकों के विनाश की प्रक्रिया बेरोकटोक चलती रही। यदि वे हस्तक्षेप न करते, तो शायद ताजमहल भी लंदन की नीलामी में बिकने के लिए रख दिया जाता।
उनकी दृष्टि में ताजमहल का संगमरमर एक 'पत्नी के मकबरे' पर बर्बाद करने के लिए बहुत मूल्यवान था।
इन परिस्थितियों में, वाराणसी के नगर-निर्माताओं से किसी भी संवेदनशीलता की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। 1774 से 1905 के बीच, वाराणसी का विध्वंस बेरोकटोक और तीव्र गति से चलता रहा।
1781 में वारेन हेस्टिंग्स को बनारस के राजा से टकराव के दौरान मंदाकिनी तालाब के किनारे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। महान प्रशासक को अंततः पीछे हटना पड़ा और एक सम्मानित नागरिक द्वारा उपलब्ध कराए गए बागीचे (माधोदास की बगिया) में शरण लेनी पड़ी, जो बड़ा गणेश मंदिर के पास था और गोला दीनानाथ के सामने स्थित था। (इसका एक स्मारक शिलालेख आज भी मौजूद है।)
इस प्रकार, मंदाकिनी तालाब वारेन हेस्टिंग्स की हार का प्रतीक बन गया और ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का भी एक अप्रत्यक्ष स्मारक बन गया।
ब्रिटिश प्रशासन विशेष रूप से वाराणसी के मंदाकिनी तालाब और बेनिया तालाब से ग्रस्त था।
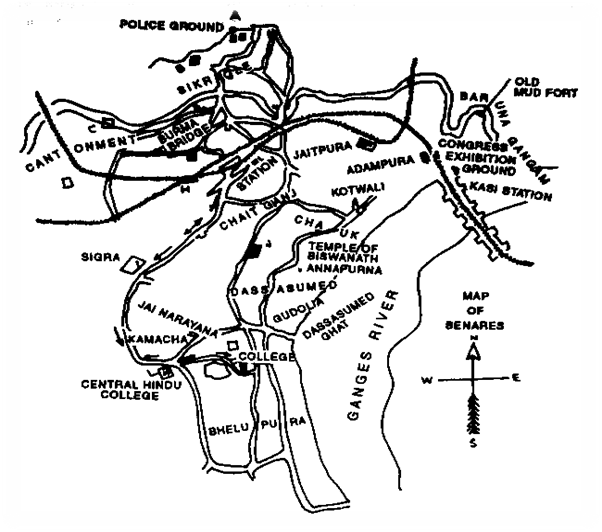
मानचित्र. 12.
अंग्रेजों द्वारा सड़क और रेलमार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त हुए वाराणसी शहर का एक मूल्यवान पुराना मानचित्र
जब नगर नियोजकों ने गंगा पर बने पुल (राजघाट रेलवे स्टेशन) को सिटी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने मंदाकिनी झील को भरने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में, उन्होंने मच्छोदरी, मच्छोदरी नाले और वरुणा-गंगा संगम के पास प्रसिद्ध नदी बंदरगाह को स्थायी रूप से सील कर दिया।
इस निर्णय ने मंदाकिनी झील के प्रवाह को बाधित कर दिया। सड़क जब बाईं ओर मुड़ी और मंड़ुवाडीह और चौक की ओर बढ़ी, तो मंदाकिनी का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया।
एक झटके में, लगभग सौ एकड़ में फैली झील, बगीचे और जंगल को समतल कर दिया गया, जिससे उसकी पूर्व की महिमा का कोई निशान नहीं बचा। अब वहाँ एक तारघर, एक पुलिस स्टेशन, एक डाकघर, एक टाउन हॉल और एक घड़ी-घर खड़ा कर दिया गया, जिन्हें प्रकृति के अनमोल उपहारों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया।
आज बड़ा गणेश मंदिर एक संकरी गली में छिपा पड़ा है, जहाँ उसका गौरवशाली अतीत लगभग भूला दिया गया है। झील के दक्षिण-पश्चिमी भाग को अब अस्पतालों और कॉलेजों के भवनों से भर दिया गया है।
इस विनाश के प्रमाण अब भी इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं:
1. इस क्षेत्र की अधिकांश इमारतें एक मंजिला हैं, जो दर्शाती हैं कि वे एक भरे गए जलाशय की मिट्टी पर खड़ी हैं।
2. यहाँ की सड़कें वाराणसी की अन्य सड़कों की तुलना में चौड़ी हैं, जो इंगित करता है कि वे पानी भरे स्थानों को पाटकर बनाई गई हैं।
3. यहाँ कोई प्राचीन संरचना नहीं पाई जाती।
4. विशेषरगंज बाजार लकड़ी और टाइल की झोपड़ियों से बना है, जिसमें कोई भारी संरचना नहीं है।
उत्तर की ओर बढ़ते हुए, वरुणा नदी और झील के बीच का क्षेत्र वाराणसी के सबसे पवित्र स्थलों में से एक था, विशेष रूप से गहड़वाल राजाओं के काल में। यहाँ कभी पाँच महान मंदिर थे। आधुनिक समय में, यह क्षेत्र लगभग उपेक्षित ही रहा।
आज जिसे जैतपुरा, आदमपुरा, जलालपुरा और विशेषरगंज कहा जाता है, वहाँ कभी वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर थे। वे ध्वस्त कर दिए गए और अब केवल उनके मलबे के ढेर शेष हैं। यदि कोई ध्यान से देखे, तो इन मंदिरों के अवशेष अभी भी अविमुक्तेश्वर मंदिर, उससे सटी मस्जिद और लाट-भैरव मंदिर की पहाड़ी पर देखे जा सकते हैं।
लाट भैरव मंदिर अब एक मस्जिद के बगल में स्थित है।
कभी इस मंदिर और मस्जिद के इमामों के बीच चढ़ावे की आय को लेकर विवाद हुआ था, जिसने हिंसक दंगे का रूप ले लिया और सैकड़ों लोग मारे गए। उसी समय लाट भैरव मंदिर के खंभे को तोड़ दिया गया, जिसकी अब केवल जड़ ही बची है।
कपालमोचन तीर्थ, जो रानी भवानी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, अब भी इस क्षेत्र में स्थित है। लेकिन अन्य ऐतिहासिक सरोवर जैसे ऋणमोचन और सापमोचन गायब हो चुके हैं।
ब्रिटिश योजनाकारों ने शहर के लिए सड़कों का निर्माण करने के नाम पर इन पवित्र सरोवरों को भर दिया, जिससे गंगा के बाढ़ के पानी का इन जलाशयों में प्रवाह सदा के लिए बंद हो गया। इस कार्य ने न केवल इन ऐतिहासिक स्थलों को मिटा दिया, बल्कि उन पुरावशेषों को भी दफना दिया, जो इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हो सकते थे।
समय कुछ
मंदिरों को पुनः स्थापित कर
सकता है, लेकिन वह कभी
उन झरनों, तालाबों और मच्छोदरी नाले को वापस नहीं
ला सकता।
15.शांत नदी बहती है
I
ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से पहले की वाराणसी और 1800 के बाद की वाराणसी पूरी तरह भिन्न थीं। वे लगभग पहचान में न आने योग्य थीं। गुप्त और पाल काल के बीच जीवन में आई भौतिक समृद्धि ने नदी-तट की इस शांत, आत्मसंयमित नगरी को गहराई से प्रभावित किया, जो एक ओर आध्यात्मिक क्षेत्र आनंदकाननम और दूसरी ओर मृगदाव से घिरी हुई थी।
पाल युग से पहले की वाराणसी (1026 ईस्वी), जिसने गौतम बुद्ध को आकर्षित किया और जहाँ (500 ईसा पूर्व) उन्होंने अपने प्रवचन शुरू किए, अब कहीं नहीं मिलती। इस नगर की शांति और सादगी ही इसका मुख्य आकर्षण थी, जो अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है।
1026 ईस्वी तक, वाराणसी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। यह नगर गोमती और वरुणा नदियों के बीच स्थित बाजारों में व्यस्त व्यापार करता था। बढ़ते व्यापारिक दबाव के कारण नगर धीरे-धीरे वरुणा नदी को पार कर गया और पुराणों में वर्णित मंदाकिनी झील तक पहुँच गया, जो आधुनिक लक्ष्मी चबूतरा और मध्यवर्ती पहाड़ियों तक फैली थी।
फिर भी, वह सक्रिय वाराणसी नगर, जिसे बुद्ध ने देखा था, सोडेपुर-भीतरी-कपिलधारा क्षेत्र के आसपास स्थित प्रतीत होता है। सारनाथ, जो बुद्ध के प्रसिद्ध धर्मोपदेशों का केंद्र बना, पहले से ही अपनी जैन परंपराओं के लिए विख्यात था।
नगर धीरे-धीरे वरुणा के दक्षिणी तट के साथ विस्तारित होता गया, जब काशी-कोसल संघर्षों के कारण लोग अधिक सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ने लगे। इस बिंदु को पुनः दोहराना आवश्यक है।
गहड़वालों (ग्यारहवीं शताब्दी की शुरुआत) के समय तक, पंचगंगा से केदार तक फैले अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के मुख्य आनंदकाननम क्षेत्र को नगरीकरण से बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया गया था। व्यापारियों ने इस निषिद्ध वन-क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं किया, जहाँ कापालिकों और अघोरों का वास था। इसके अलावा, व्यापारी वहीं टिके रहते जहाँ व्यापार होता था। वन क्षेत्रों में उनका कोई आकर्षण नहीं था।
नदियाँ और धाराएँ झीलों और तालाबों में प्रवाहित होती रहीं। वन क्षेत्रों में संन्यासी, विद्वान, छात्र और योगी अपनी साधना और अध्ययन में संलग्न रहते। संत ध्यान और तपस्या के लिए एकांत खोजते रहे, और कवि वाराणसी की आध्यात्मिक विशेषताओं का गुणगान करते रहे, जहाँ सभी प्रकार की दार्शनिक विचारधाराएँ और योग पद्धतियाँ पनपने और विकसित होने के लिए स्वतंत्र थीं।
गहड़वालों के काल के बाद जो परिवर्तन वाराणसी में आए, वे मुख्यतः दो आंतरिक राजनीतिक संघर्षों के कारण थे—
1. पहले कोसल राज्य के हमले
2. फिर बौद्ध-जैन टकराव
इन संघर्षों के कारण, वरुणा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र, जो आधुनिक गाज़ीपुर तक फैला था, लगभग नष्ट-भ्रष्ट हो गया। जनसंख्या और व्यापारिक गतिविधियाँ दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गईं। धीरे-धीरे, वाराणसी का नगर क्षेत्र वरुणा नदी के दक्षिणी तट और गंगा नदी के किनारे पंचगंगा तक फैल गया।
फिर भी, मुख्य अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ और उनकी पश्चिमी घाटियाँ लगभग अछूती रहीं। वन हरे-भरे रहे और शांति बनी रही। जलधाराएँ तालाबों और अंततः गंगा में समाहित होती रहीं। गंगा के जल स्तर में वृद्धि और गिरावट से तालाबों और धाराओं का स्तर प्रभावित होता रहा। अध्ययन केंद्र फले-फूले, विद्वान अपने प्रवचन देते रहे और संत अपनी साधना में मग्न रहे।
परिवर्तन तब आया जब अफगानिस्तान से पठानों ने अचानक आक्रमण किया (1026-1094)। उस समय की वाराणसी, विशेष रूप से मंदिरों की संपत्ति, इन लुटेरों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। वे मुख्य रूप से लूटपाट में रुचि रखते थे, धर्म केवल एक सुविधाजनक बहाना था।
इससे बचने का कोई उपाय नहीं था। 1024 और 1658 के बीच, भारत के हिंदू समाज को, विशेष रूप से वाराणसी, वृंदावन और मथुरा को, एक भयानक परिवर्तन से गुजरना पड़ा। वाराणसी के लोग मूक पीड़ा और आतंक में जीते रहे, जब तक कि अकबर का शासन नहीं आया।
यह 1556 का वर्ष था।
1567 से, अकबर, जहाँगीर और दारा शुकोह (जो संयोगवश अवध के मुगल गवर्नर थे और जिनका मुख्यालय वाराणसी में था) की नीतियों के कारण पीड़ित शहर को एक सुखद राहत मिली। वाराणसी धीरे-धीरे पुनर्जीवित होने लगी। पुरानी, शास्त्रों में वर्णित वाराणसी धीरे-धीरे लुप्त होने लगी और एक नई वाराणसी का निर्माण हुआ, जो धीरे-धीरे विश्वनाथ पहाड़ी से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गई, जहाँ नए राजपूत और जाट समुदायों ने पुराने भरा-शिव (वाकाटक पूर्वज) और परंपरागत समाज से बहिष्कृत लोगों के साथ मिलकर बसावट शुरू की।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि शास्त्रों में इस क्षेत्र, अर्थात् आनंदकाननम, को गृहस्थों के लिए निषिद्ध घोषित किया गया था।
उत्तरी और पारंपरिक वाराणसी की आबादी, जिसे सामाजिक बाधाओं के कारण हिंदू धर्म से इस्लाम में जबरन परिवर्तित होना पड़ा था, और जिसने अपनी पारंपरिक व्यापारिक संघों को खो दिया था, एक नए निवास, एक नए जीवन और एक नई पहचान की तलाश में थी। इस कारण मुस्लिम बस्तियाँ मुख्य रूप से खंडहर हो चुके मंदिरों के पास उत्तर में और परित्यक्त पश्चिमी पहाड़ी ढलानों पर दक्षिण में बसने लगीं। इनमें प्रमुख क्षेत्र थे—खालिसपुरा, मदनपुरा, देवनाथपुरा, रेवती तालाब, काली महल, औरंगाबाद और अर्दली बाजार। (अंतिम बस्ती ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उनके सेवकों के लिए बसाई गई थी।)
इसके बाद 1560 में काला पहाड़ और 1658 में औरंगजेब का शासन आया, जिनके आक्रमणों ने वाराणसी को पूरी तरह से झकझोर दिया। अब तक हिंदू समुदाय मुगलों के साथ सहयोग कर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की कोशिश कर रहा था। कई खंडहर मंदिरों की मरम्मत की गई थी, बाजार पुनः व्यवस्थित हुए थे, संचार सुरक्षित हुआ और व्यापारी अपने माल का सुरक्षित रूप से लेन-देन कर सकते थे।
लेकिन औरंगजेब के शासन के साथ सब कुछ बदल गया। चूँकि दारा शुकोह ने वाराणसी को विशेष संरक्षण दिया था और यहाँ संस्कृत और उपनिषदों की शिक्षा ली थी, इसलिए औरंगजेब को इस शहर से विशेष द्वेष था। उसने आदेश दिया कि—
1. सभी मरम्मताधीन मंदिरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए।
2. नवनिर्मित विश्वनाथ मंदिर (जो अकबर के शासनकाल में नारायण दत्त द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था) को ध्वस्त कर दिया जाए, साथ ही प्रसिद्ध पंचगंगा परिसर में स्थित बिंदुमाधव मंदिर को भी।
दोनों मंदिरों को भव्य मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया। काफिर दारा शुकोह के ‘पापों’ को मिटाना आवश्यक था। यदि वाराणसी में ‘दारानगर’ था, तो औरंगजेब इसे ‘आलमगीर नगर’ में बदलना चाहता था।
1627 के बाद, वाराणसी में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। उत्तरी वाराणसी से दक्षिण की ओर जनसंख्या का विस्थापन हुआ, जिससे नई वाराणसी अस्तित्व में आई और अपने अमर इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई।
1585-1660 और 1707-1781 की अवधि वाराणसी के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस दौरान राजपूतों और मराठों ने घाटों का निर्माण किया, जिससे वाराणसी का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। इस दौरान निर्मित वाराणसी अब तक विश्व वास्तुकला के लिए एक अद्भुत उदाहरण बनी हुई है।
II
उपरोक्त विश्लेषण ठोस तथ्यों पर आधारित है। आइए, नदी के घाटों की सूची प्रस्तुत करें और जहाँ संभव हो, उनके निर्माण की तिथियों का उल्लेख करें। यह हमारे दृष्टिकोण की पुष्टि करेगा (यदि और प्रमाण आवश्यक हों) कि वर्तमान वाराणसी आधुनिक विकास का परिणाम है; कि प्राचीन वाराणसी पूरी तरह भुला दी गई है, जिसमें राजघाट का किला भी शामिल है; कि जैन, बौद्ध और प्रारंभिक हिंदू वाराणसी वरुणा नदी के उत्तरी तट पर छूट गई है; और कि मौर्य, गुप्त और शुंग काल की व्यावसायिक वाराणसी अब वाराणसी के रूप में नहीं जानी जाती। वही वास्तविक वाराणसी थी।
इन तथ्यों को दो चरणों में प्रस्तुत करना होगा:
1. 1565-1627
2. 1734-1787
1565 और 1627 के बीच, पहले चरण में, अधिकांश घाटों का निर्माण राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा किया गया था।
वरुणा नदी के पुराने तट को छोड़कर वाराणसी के नए तट का निर्माण करने का विचार संभवतः कई कारकों से प्रेरित था।
प्रमुख कारणों में से एक यह था कि वरुणा तट पूरी तरह नष्ट हो चुका था। दिल्ली के अफगान शासकों के बार-बार होने वाले आक्रमणों और लूटपाट के उद्देश्य से आए हमलावरों ने दोनों तटों को निर्जन बना दिया था। सारनाथ सदियों पहले ही विलुप्त हो चुका था। भीतरी, सोडेपुर और गोमती संगम के पास की बस्तियाँ भी लगातार आक्रमणों, सुरक्षा की कमी और व्यापार में गिरावट के कारण उजड़ गई थीं। शहर दक्षिण की ओर खिसक गया, यह आशा करते हुए कि विनाश की लपटें वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी।
दूसरा कारण यह था कि अत्यधिक लोकप्रिय और सम्मानित मंदिरों के विध्वंस की भयावहता ने किसी भी प्रकार के पुनर्निर्माण को असंभव बना दिया था—चाहे वह स्थापत्य, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक दृष्टि से हो। ऐसे में इन क्षेत्रों को छोड़ देना ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प था।
तीसरा कारण यह था कि इन क्षेत्रों की जनसंख्या की प्रकृति और संरचना बदल चुकी थी। हालाँकि, कुछ हिंदू परिवार अब भी वहाँ बसे हुए थे, लेकिन अधिकांश प्राचीन आबादी नए धर्म में परिवर्तित हो चुकी थी। वे नए मंदिरों के निर्माण को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ जुड़े बाजार भी धीरे-धीरे लुप्त हो गए। नए मंदिरों के निर्माण के साथ-साथ बाजार भी नए स्थानों पर स्थानांतरित हो गए।
लगातार उपेक्षा के कारण वरुणा की नौवहन क्षमता भी समाप्त हो चुकी थी। नदी की उथली धारा ने इसके किनारे पुनः बसने या व्यापार और उद्योग में निवेश को हतोत्साहित कर दिया।
इसलिए, वाराणसी के पुनर्निर्माण को एक नए तट के साथ, विशेष रूप से पहाड़ी ऊँचाई पर करने का निर्णय व्यावहारिक प्रतीत हुआ। यह क्षेत्र अव्यवस्थित और अनिश्चित पहचान वाले लोगों से भरा हुआ था, जिनकी नागरिकता और व्यवसाय संदिग्ध थे। ऐसे में इस क्षेत्र को पूरी तरह साफ कर नया वाराणसी बसाना व्यावहारिक निर्णय था।
प्रथम चरण के दौरान कई घाटों का निर्माण हुआ। इस ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत पूरी तरह अप्रत्याशित है।
हमने पहले एक अंग्रेज़ यात्री राल्फ़ फिच का उल्लेख किया था। जब उन्होंने वाराणसी का दौरा किया, तब शहर अकबर और जहाँगीर के शासनकाल के दौरान पहली बार लूट-मार और आक्रमणों से राहत महसूस कर रहा था।
पुनर्निर्माण राजा मान सिंह और राजा टोडरमल की ऊर्जावान पहल के कारण संभव हुआ।
फिच ने वाराणसी को एक व्यस्त नगर के रूप में पाया, जो सूती वस्त्रों और हस्तशिल्प के व्यापार में संलग्न था। आज फिच की डायरी को पढ़ना ऐसा लगता है जैसे हम उस समय के वाराणसी के जीवन का विस्तृत चित्र देख रहे हों—एक ऐसा नगर जो दर्शन और अंधविश्वास, संतों और ठगों, भिखारियों और बैलों, धूर्तों और व्यापारियों, विद्वानों और अपराधियों से भरा हुआ था।
फिच ने वाराणसी के घाट नहीं देखे। उस समय गंगा में स्नान करने वाले लोग मिट्टी, कीचड़ और कंकड़-पत्थर से भरे ढलानों से उतरते थे। उन्होंने किसी घाट का नाम नहीं लिया, शायद इसलिए क्योंकि उस समय घाट स्पष्ट रूप से निर्मित नहीं थे। यहाँ तक कि श्मशान घाटों के भी कोई निश्चित नाम नहीं थे।
सौभाग्य से, हमारे पास एक और ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध है—गिर्वाण पदमंजरी (Girvana Padamanjari, Blossoms of Divine Talk), जिसे वरदराज (1600-1660) ने लिखा था।
इस पुस्तक में कुछ घाटों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार हैं:
1. राजघाट – वरुणा संगम के पास, पुराने किले के नीचे।
2. ब्रह्मघाट
3. दुर्गाघाट
4. बिंदुमाधव घाट
5. त्रिलोचन घाट – गया घाट के पास एक प्रसिद्ध स्नान स्थल।
6. अग्निश्वर घाट – राम घाट के पास।
7. नागेश्वर घाट – अब इसे ‘भोंसला घाट’ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नागपुर के भोंसला शासकों ने इसका व्यापक पुनर्निर्माण किया था।
8. वीरेश्वर घाट – वर्तमान मणिकर्णिका घाट के पास।
9. सिद्ध विनायक घाट – इस विनायक की प्रसिद्धि के कारण अब भी एक क्षेत्र ‘सिद्ध विनायक’ के नाम से जाना जाता है।
10. जरासंध घाट – अब यह नाम प्रचलित नहीं है। वर्तमान में इसे मीर घाट के रूप में जाना जाता है, जहाँ मीर अली ने अपना किला बनवाया था।
11. बृध्दादित्य घाट – वाराणसी के सूर्य मंदिरों से संबंधित, विशालाक्षी मंदिर के पास, मीर घाट से हटकर।
12. सोमेश्वर घाट – त्रिपुरा भैरवी मंदिर के पास।
13. रामेश्वर घाट – वर्तमान में मानमंदिर के पास।
14. लोलार्क घाट – असि के पास लोलार्क कुंड के समीप।
15. दशाश्वमेध घाट – यह अब भी प्रयोग में है, लेकिन इसे पत्थर की सीढ़ियों से बाद में पक्का किया गया।
16. चौसठी घाट – यह प्रसिद्ध घाट अब भी प्रयोग में है।
17. सर्वेश्वर घाट – पांडेय घाट के पास, जिसे हाल ही में पुनर्निर्मित किया गया है।
18. केदार घाट – यह भी एक प्रसिद्ध घाट है और अभी भी उपयोग में है।
गिर्वाण पदमंजरी में घाटों के साथ-साथ कुछ स्थानीय क्षेत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जो पूरी तरह से तीर्थस्थलों के इर्द-गिर्द विकसित हुए थे।
ये क्षेत्र इस प्रकार हैं:
● स्वर्गद्वार प्रवेश
● मोक्षद्वार प्रवेश
● गंगा-केशव
● असि-संगम
● वरुणा-संगम
● लोलार्क
इनमें से अधिकांश घाट और क्षेत्र धार्मिक महत्व के केंद्र थे।
मणिकर्णिका और विश्वेश्वर मंदिर के आसपास के घाटों में त्रिपुरा भैरवी गली प्रमुख थी, जहाँ अब भी लगभग सभी तांत्रिक देवी मंदिर छोटे रूप में मौजूद हैं।
इस क्षेत्र में प्राचीनतम निर्माण मानमंदिर घाट पर स्थित वराही तांत्रिक मंदिर है। इसे राजा मान सिंह ने बनवाया था, और उनके वंशज जय सिंह द्वितीय ने इसे वेधशाला के रूप में उपयोग किया।
यह वेधशाला जयपुर, दिल्ली और उज्जैन में बनाई गई अन्य वेधशालाओं के समान थी। यह घाट वाराणसी की अनूठी संरचनाओं में से एक है।
इन घाटों के निर्माण के साथ, 1660 तक वाराणसी के पुनर्निर्माण और विस्तार का पहला चरण पूरा हुआ।
III
द्वितीय चरण (1707-81) दिल्ली सम्राट की रोहिला सरदार द्वारा अपमानजनक पराजय से आरंभ हुआ। इस कठिन परिस्थिति में उसने मराठा सरदार महादजी सिंधिया से सहायता मांगी। पेशवा ने विशेष रियायत के रूप में वाराणसी, मथुरा और वृंदावन के पुनर्निर्माण की अनुमति लेकर सहायता प्रदान की।
इस रियायत ने वाराणसी के कंकरीले पहाड़ी तट को संवारने और पूरे 2 किमी क्षेत्र को पत्थर की सीढ़ियों से सुसज्जित करने की प्रेरणा दी। भारी पत्थर के बुर्ज बनाए गए ताकि मानसून में नदी की उग्रता के विरुद्ध निर्माण को सुरक्षित रखा जा सके।
कुछ स्थानों पर पहाड़ियाँ 110 फीट से भी अधिक ऊँचाई तक जाती थीं। उनकी खड़ी और खतरनाक ढलान ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता को चुनौती दी। लेकिन साधारण संरचनाओं के बजाय, वास्तुकारों की कल्पना ने इन पहाड़ियों को महलों, उद्यानों और मंदिरों से अलंकृत किया, जो आज भी दर्शकों को प्रेरित और प्रभावित करते हैं।
इन कुशल शिल्पकारों की निपुणता को देखकर आश्चर्य होता है, जो भारत के विभिन्न भागों से यहाँ आए और अपनी निर्माण-कला का प्रदर्शन किया।
इस दूसरे चरण में बने घाट इस प्रकार हैं:
असि घाट हमेशा से गंगा के तीन प्रमुख स्नान-स्थलों में गिना जाता है, अन्य दो हैं मणिकर्णिका और वरुणा संगम। आश्चर्यजनक रूप से, असि और वरुणा घाट आज भी पत्थर की सीढ़ियों से सुसज्जित नहीं हैं।
संभवतः यह नदी की धारा के उतार-चढ़ाव के कारण है। फिर भी, असि और वरुणा दोनों को पवित्र स्नान-स्थल माना जाता है। असि घाट के पास प्रसिद्ध लोलार्क कुंड स्थित है, और वरुणा घाट अपने केशव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
असि घाट के बाद तुलसी घाट आता है। यह घाट अत्यधिक कमज़ोर बनाया गया था, जिससे यह नदी की तीव्र धारा को झेल नहीं सका और शीघ्र ही जीर्ण-शीर्ण हो गया। संत तुलसीदास की स्मृति के कारण, यह घाट पूरी तरह विस्मृत नहीं हुआ और आज भी अस्तित्व में है।
हाल ही में तुलसी घाट के पास एक नया घाट बनाया गया, जो एक आधुनिक संत मा आनंदमयी को समर्पित है और काफी लोकप्रिय हो चुका है।
चेतसिंह किला का कोई घाट नहीं है, यद्यपि इसका नदी तट एक उत्कृष्ट घाट के रूप में निर्मित था, जहाँ राजा की नौकाएँ लंगर डालती थीं। वास्तविक स्नान पास के शिवाला घाट पर किया जाता था, जिसे समतल रूप में निर्मित किया गया था ताकि जल प्रवाह बाधित न हो।
इसके बाद हनुमान घाट आता है, जो हनुमान के अलावा रुरु भैरव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रुरु भैरव को कुत्तों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर श्मशानों के आसपास रहते थे।
हनुमान घाट के पास स्थित हरिश्चंद्र घाट वाराणसी का प्राचीनतम श्मशान घाट है। एक समय यह मुख्य श्मशान घाट हुआ करता था, जब तक कि मणिकर्णिका घाट को वैकल्पिक रूप से स्थापित नहीं किया गया।
हरिश्चंद्र घाट की प्रसिद्धि यहाँ के अघोरी-तांत्रिक संत केनाराम के कारण भी है। उनका स्थान (आश्रम) पास के शिवालय क्षेत्र में है, जो 1900 तक घने जंगलों से घिरा हुआ था।
हरिश्चंद्र घाट के बाद केदार घाट आता है। यह सुदृढ़, ऊँचा और शक्तिशाली घाट है, जो नदी की धारा को नियंत्रित कर उसका प्रवाह शांत करता है। इसे मद्रास के तिरुनेलवेली के कुमारास्वामी ने अकबर के शासनकाल में बनवाया था। लेकिन केदारनाथ मंदिर का उल्लेख काशी खंड में मिलता है, जिसमें वशिष्ठ नामक ब्राह्मण द्वारा हिमालय के केदारनाथ की शक्ति को यहाँ स्थापित करने की कथा है। यह वाराणसी का एकमात्र मंदिर है, जिसे कभी अपवित्र नहीं किया गया।
इसके बाद चौकी घाट आता है, जो शायद नदी कर-संग्रहण केंद्र रहा होगा। यह घाट लंबे समय से जर्जर स्थिति में था, लेकिन हाल ही में नगर प्रशासन ने इसकी मरम्मत करवाई है।
इसके बाद घाटों का एक लंबा भाग आता है, जहाँ कोई स्नान नहीं करता। यह संभवतः यहाँ के बड़े नाले के कारण है, जो जल को प्रदूषित करता है। धोबी इस स्थान का उपयोग कपड़े धोने के लिए करते हैं।
हरिश्चंद्र और केदार घाट के बीच दो छोटे घाट स्थित हैं:
● लाली घाट – इसे किसी लाल शाह नामक फौजदार ने बनवाया था।
● लक्ष्मी घाट – एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण घाट।
● विजयनगर घाट – दक्षिण भारत के विजयनगर राजाओं द्वारा निर्मित।
चौकी घाट के बाद सोमेश्वर घाट आता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, यद्यपि यहाँ का सोमेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
मानसरोवर घाट का निर्माण अंबर के राजा मान सिंह ने करवाया था। मराठा और बंगाली धनी व्यक्तियों द्वारा बनाए गए कई घाट समय के साथ नष्ट हो गए। केवल अमृत राव घाट, जिसे पेशवा विनायक राव ने बनवाया था, आज भी भव्य स्थिति में मौजूद है और इसे प्रायः राजा घाट कहा जाता है।
इसके बाद, कुछ अन्य घाटों पर धोबी और भैंसे काबिज हैं।
गंगा महल घाट और पांडेय घाट प्रसिद्ध पांडेय परिवार के योगदान हैं, जो वाराणसी में तीर्थयात्रियों के मार्गदर्शक के रूप में एकाधिकार रखते हैं।
इसके बाद चौसठी घाट आता है, जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है।
राणा महल घाट राजस्थान के उदयपुर के राणाओं द्वारा निर्मित है। इसके बाद बिहार के महाराजा दरभंगा का भव्य महल स्थित है, जिसका निर्माण प्रथम विश्वयुद्ध के बाद हुआ, जबकि महल उन्नीसवीं शताब्दी का है।
मुंशी श्रीधर प्रसाद ने एक सुंदर घाट बनवाया, जो अब मुंशी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यह घाट अत्यधिक प्रभावशाली है और इसके पास ही अहिल्या बाई घाट स्थित है।
इन घाटों के साथ वाराणसी के घाटों के बाद के निर्माण कार्य समाप्त हो जाते हैं। इनमें से कोई भी घाट सोलहवीं शताब्दी में अकबर के शासन से पहले अस्तित्व में नहीं था।
दशाश्वमेध घाट से पंचगंगा घाट तक के प्राचीन घाटों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इनमें से अधिकांश घाट मुगल शासनकाल में बने थे, लेकिन श्रद्धालु इन्हें पवित्र ग्रंथों में उल्लिखित होने के कारण अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।
इसके विपरीत, चौकी घाट (केदार के उत्तर) से मणिकर्णिका घाट के बीच के सभी घाट (दशाश्वमेध और प्रयाग को छोड़कर) मुगल काल के बाद बने थे।
पंचगंगा और आदिकेशव घाटों के बीच स्थित घाटों की चर्चा पहले ही हो चुकी है। इनका निर्माण मुख्यतः मराठों के उत्थान और मुगलों के पतन के दिनों में हुआ।
इस प्रकार, वाराणसी का बारहवीं शताब्दी से पहले और अठारहवीं शताब्दी के बाद का स्वरूप पूरी तरह भिन्न था।
आधुनिक घाटों के निर्माण के बावजूद, वाराणसी की आध्यात्मिक गरिमा कभी भी अपने प्राचीन, शांत और गंभीर स्वरूप को पुनः प्राप्त नहीं कर सकी।
जो वाराणसी बुद्ध के पूर्व काल से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक थी, उसे केवल वनों, आश्रमों, उद्यानों और संतों के ध्यान स्थलों के रूप में ही समझा जा सकता है।
"वह गौरवशाली चंद्रमा सदा के लिए अस्त हो गया,
फिर कभी लौटकर आने के लिए नहीं!..."
– रवींद्रनाथ टैगोर
Notes
1. स्वयंभू लिंगम
हिंदू परंपरा में "स्वयंभू" (स्वयं उत्पन्न; स्वयं प्रकट) शब्द का उल्लेख प्रायः लिंगम के संदर्भ में किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर और वाराणसी के केदारेश्वर इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत में इस प्रकार के सैकड़ों लिंगम विद्यमान हैं। प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग (बारह प्रकाशित लिंगम) विशेष रूप से प्रतिष्ठित हैं।
लेकिन वास्तव में स्वयंभू लिंगम क्या होता है?
भक्तगण प्रायः इस धारणा से प्रभावित होते हैं कि भगवान ने करुणावश अपने अनुयायियों के लिए स्वयं को लिंग रूप में प्रकट किया। यदि ऐसा भौतिक रूप से संभव होता, तो संसार में न कोई कष्ट होता और न ही मृत्यु।
दुर्भाग्यवश, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के नियम इतने सरल नहीं हैं। चमत्कार सदा और हर परिस्थिति में घटित नहीं होते। जो लोग चमत्कार की अपेक्षा करते हैं, वे कभी-कभी अप्रत्याशित घटनाओं से चकित हो जाते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक उन्हें आत्म-परिकल्पना, भ्रम या इच्छित सोच के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ऐसे चमत्कार बहुत कम प्रमाणिकता प्राप्त करते हैं।
फिर भी, स्वयंभू लिंगम वास्तव में मौजूद हैं, और इसकी लोकप्रिय मान्यता को पूरी तरह से कल्पना मात्र नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे कुछ तार्किक आधार अवश्य है।
स्वयंभू लिंगम का मूल और उत्पत्ति
हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि लिंगम को देवता के रूप में पूजने की परंपरा आदिवासी सभ्यताओं द्वारा विकसित और लोकप्रिय बनाई गई थी। ये लोग प्रजनन और जीवन की वृद्धि के रहस्य से विस्मित होते थे और इस चमत्कारिक शक्ति के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। वे जीवन की निरंतरता के लिए अत्यंत कृतज्ञ थे और इसे उत्पन्न करने वाली शक्तियों की पूजा करने लगे।
किन्तु, उन्होंने अपने विचारों और मान्यताओं को त्रि-आयामी मूर्तियों में ढालने में हिचकिचाहट दिखाई। अतः, वे अपने स्वप्न-देवता को प्राकृतिक रूप में प्रकट होते हुए देखने लगे—विशेषकर गुफाओं और चट्टानों में बनने वाली दरारों और जलधाराओं के रूप में।
गुफाओं और चट्टानों में बनी दरारें उनके लिए सृजन-प्रक्रिया का प्रतीक बनीं, और पर्वतों की चोटियों और शंक्वाकार संरचनाओं ने उनके लिए उसी प्रक्रिया के एक अन्य पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। एक ने स्त्री-ऊर्जा का प्रतीक दिया, तो दूसरे ने पुरुष-ऊर्जा का।
स्वयंभू लिंगम की खोज और प्रतिष्ठा
● पत्थर की मूर्तियाँ गढ़ने से बहुत पहले, जब मानव ने पहली बार मिट्टी, पत्थर और अन्य माध्यमों में मानव-आकृतियाँ उकेरनी शुरू की थीं, उससे भी पहले, सरल जीवन जीने वाले लोगों ने वृक्षों, खेतों में हल द्वारा बनी रेखाओं, और गाँवों के समीप स्थित प्राकृतिक टीलों को पवित्र मान लिया।
● इन स्थलों पर वे अज्ञात शक्तियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने लगे।
● कभी-कभी, उन्होंने पहाड़ियों से निकली प्राकृतिक शंक्वाकार संरचनाओं की खोज की और उन्हें "स्वयं प्रकट" मान लिया।
● इन स्थलों को संरक्षित किया गया और उनकी श्रद्धा से प्रतिष्ठा बढ़ती गई।
● इस प्रकार के प्राकृतिक रूप से निर्मित लिंगम ही "स्वयंभू लिंगम" के रूप में प्रतिष्ठित हुए।
प्रसिद्ध स्वयंभू लिंगम:
भारत में कई स्वयंभू लिंगम प्रतिष्ठित हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
● बारह ज्योतिर्लिंग (द्वादश ज्योतिर्लिंग)
● भुवनेश्वर (ओडिशा)
● केदारेश्वर (वाराणसी)
● केदारनाथ (उत्तराखंड)
● पशुपतिनाथ (नेपाल)
● महाकालेश्वर (उज्जैन)
विशेष जानकारी:
● सोमनाथ स्वयंभू लिंगम नहीं है, जबकि महाकालेश्वर (उज्जैन) स्वयंभू लिंगम है।
● केदारनाथ और बद्रीनाथ दो अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
इस प्रकार, स्वयंभू लिंगम की अवधारणा किसी चमत्कारी घटना से अधिक, एक प्राकृतिक घटना के प्रति मानव की श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना का परिणाम है।
2. वाराणसी के नामों का शास्त्रीय संदर्भ
A. स्कंद पुराण के काशीखंड के 26वें अध्याय में उल्लेख है:
"... अविमुक्तमिदं क्षेत्रं कदराब्य भुवस्थले
परं प्रतिष्ठामापन्नं
मोक्षदं चाभवत्कथम्
कथमेषा त्रिलोकीभ्यां
गीयते मणिकर्णिका
तत्रासीत्किं पुरा
स्वामिन्यदा नामार
निम्नगा...."
ऋषि अगस्त्य ने स्कंद (कार्तिकेय), जो पार्वती और शिव के पुत्र हैं, से यह प्रश्न पूछा:
"... यह भूमि, जिसे अविमुक्त कहा जाता है, किस समय प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई? यह मोक्ष प्रदान करने वाला स्थान कैसे और कब घोषित हुआ? इसे मणिकर्णिका के रूप में गाने का क्या कारण है, और तीनों लोकों में इसे इस नाम से क्यों जाना जाता है? और उस समय, जब गंगा की धारा यहाँ नहीं थी, तब वहाँ कौन रहता था?" (श्लोक 2-3)
स्कंद ने इस प्रश्न के उत्तर में जो कहा, उसे उन्होंने अपना कथन नहीं बताया। वे कहते हैं कि यह प्रश्न स्वयं माँ (पार्वती) ने भगवान शिव से पूछा था और जो उत्तर उन्होंने माँ को दिया था, वही दोहराया जा सकता है:
"एवं अप्राक्षीदम्बिका हरं
यथा च देवदेवेन सर्वज्ञेन निवेदितम्
जगन्मातुः पुरस्तात्..."
"अंबिका (पार्वती) ने यही प्रश्न हर (शिव) से पूछा था, और मैं वही तुम्हें बता सकता हूँ..."
"वाराणसीति काशीति
रुद्रवासेति प्रभो
अवापा नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी..."
"इस नगर ने वाराणसी, काशी, रुद्रवास आदि इतने नाम कैसे प्राप्त किए?" (श्लोक 3-4)
"ततस्तदैकालेनापि स्वैरं विहरतामया
स्व विग्रहात्स्वयं
सृष्टा स्वशरीरानपायिनी
प्रधानं प्रकृतिं त्वञ्च माया गुणवतीं
पराम्।"
"बाद में, जब मैं (शिव) अकेला भ्रमण कर रहा था, तो मैंने अपनी ही सत्ता से प्रधान-प्रकृति को उत्पन्न किया, जिसमें गुण और माया समाहित थे, एक ऐसा ब्रह्मांडीय तत्व जो सांसारिक व्याख्या से परे है।" (श्लोक 21-22)
B. ज्ञानवापी
वापी क्यों? वापी क्या है?
● "तड़ाग" तालाब या बड़ी झील को कहते हैं, जैसे कि रेओरी या रेवतीतालाब।
● "कूप" कुएं को कहते हैं, जैसे कि धर्मकूप या कालकूप।
● "वापी" को चारों ओर से सीढ़ियों से घिरा जलस्रोत माना जाता है। उदाहरण के लिए, लोलार्क को वापी कहा जा सकता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध वापी ज्ञानवापी है।
● कालिदास के "मेघदूतम्" में उल्लेख है:
"वापी चास्मिन् मरकत-शिला-बद्ध-सोपान-मार्गः"
("इस वापी के चारों ओर
मरकत (पन्ना) जैसी शिलाओं से
बनी सीढ़ियाँ हैं।")
C. महाश्मशान
(क)
"श्मशानानां च
सर्वेषां श्मशानं यत्परं महत्
पीठनं परमं पीठं ऊषरणं महोषरम्।"
(श्लोक XXXV.2)
"सभी श्मशानों में यह अद्वितीय है, यह एक पवित्र पीठ (काशी में), एक महान पीठ, और सबसे निर्जन स्थानों में सर्वोच्च है।"
(ख)
"स्म शब्देन शवः प्रोक्तः सनं
शयनमुच्यते
निर्वचंति श्मशानार्थं मुने शब्दार्थकोविदाः।" (श्लोक
XXX.103)
"(निरुक्त के अनुसार) 'स्म' का अर्थ शव (मृत शरीर) होता है, और 'सनं' का अर्थ लेटना होता है। इस प्रकार, व्याकरण के ज्ञानी श्मशान का यही अर्थ निकालते हैं।"
D. रुद्रवास
"रुद्र दश-दश प्राच्य-वाची प्रत्यग उदक
स्थितः
ऊर्ध्वादिक्ष्थश्च ये
रुद्राः पठ्यन्ते वेदवादिभिः।
असंख्यात सहस्राणि ये रुद्रा अधि
भू-तले
तत्सर्वेभ्याधिकः काश्यां
जन्तवो रुद्र-रूपिणः।
रुद्रवासः ततः प्रोक्तम्-अविमुक्तं घटोद्भव।"
(श्लोक XXX.97-101)
"पृथ्वी के दस दिशाओं को दस रुद्रों ने सुरक्षित किया है। ग्यारहवाँ रुद्र शिखर की रक्षा करता है। वेदों में इन रुद्रों का वर्णन किया गया है। इस पृथ्वी पर असंख्य रुद्र हैं, लेकिन काशी में जो जीवित रूप में निवास करते हैं, वे सभी से श्रेष्ठ हैं। इसलिए इसे रुद्रवास कहा जाता है। हे घटोद्भव (अगस्त्य), ये कभी इस स्थान को नहीं छोड़ते।"
E. आनंदकानन
ब्रह्मांडीय शक्तियों के मिलन का उल्लेख
इस ग्रंथ के छठे अध्याय में ब्रह्मांडीय शक्तियों के मिलन को स्पष्ट और जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है।
● आदिप्रकृति (मूलभूत शक्ति) से पुरुष की उत्पत्ति हुई।
● पुरुष के संकल्प से शक्ति (सृजनात्मक प्रवृत्ति) का उद्भव हुआ।
● इस शक्ति को प्रकृति कहा गया, जिसमें गुण और चेतना की शक्ति समाहित थी।
● यह प्रक्रिया रामणता (आनंदमय क्रीड़ा), लीला (सृजनात्मक खेल), और चेतना के गतिशील गुणों के रूप में व्याख्यायित की गई।
● इसे सांसारिक संदर्भों में "यौन शक्ति" के रूपक में व्यक्त किया गया, लेकिन वास्तव में यह सृजन-शक्ति का प्रतीक है।
श्लोक 24-35:
"स शक्ति: प्रकृतिः प्रोक्ता सः पुमान ईश्वरः परः
ताभ्यां च रममाणाभ्यां तस्मिन क्षेत्रे घटोद्भव।"
"वह शक्ति (प्रकृति) है, और वह पुरुष (ईश्वर) है। इन दोनों के क्रीड़ा क्षेत्र में, हे अगस्त्य, यह आनंदकानन विद्यमान है।"
F. काशी
"अविमुक्तं महाक्षेत्रं न मुक्तं शंभुना
क्वचित्
निर्वाण-कासनात्-यत्र काशीति प्रथिता
पुरी।" (श्लोक
XXIX.5)
"अविमुक्त एक महान क्षेत्र है, जिसे कभी शंभु (शिव) ने नहीं छोड़ा। निर्वाण (मोक्ष) की प्राप्ति के कारण इसे काशी के रूप में जाना जाता है।"
काशीखंड के अनुसार वाराणसी के तीन प्रमुख लिंगम
"हृदये तस्य जायन्ते त्रिणि लिंगान्यासंशयम्।" (श्लोक XXX.4)
"निस्संदेह, उसके हृदय से तीन लिंग उत्पन्न होते हैं।"
ये तीन लिंग कौन-से हैं?
1. कृत्तिवासेश्वर
2. ओंकारेश्वर
3. त्रिलोचन
विशेष:
● यहाँ विश्वेश्वर (विष्णुवर) लिंग का उल्लेख नहीं है।
● ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रुद्रीय (गैर-वेदिक भैरव-संप्रदाय) से जुड़े लोग भैरव-रूप विश्वनाथ से अधिक जुड़े हुए थे।
● कृत्तिवासेश्वर का मंदिर सबसे ऊँचा और विस्तृत था, और इसे वाराणसी के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता था।
"कृत्तिवासेश्वरस्यैषा महा-प्रसाद-निर्मितिः
यं दृष्ट्वापि नरो दूरात कृत्तिवास पदं लभेत।"
(श्लोक XXXIII.62-63)
"इस भव्य मंदिर को देखकर भी मनुष्य कृत्तिवासेश्वर की शरण प्राप्त कर सकता है।"
संदर्भ सूची
|
पुस्तक |
पृष्ठ |
पुस्तक |
पृष्ठ |
|
अब्दुल लतीफ |
233 |
अभिनवगुप्त |
110 |
|
आदमपुरा |
277 |
अधाई कंगूरे, मस्जिद |
215 |
|
अधाई-दिन-का-झोपड़ा |
215 |
आदि केशव |
35, 62, 122, 201, 205, 213, 218, 246, 294; केशवादित्य 58 |
|
आदि महादेव |
62 |
आदि शंकर |
192; सौंदर्य लहरी 162 |
|
आदि-विश्वनाथ पर्वत |
194 |
अफगानिस्तान, पठानों का अचानक आक्रमण |
284 |
|
मरणोत्तर संस्कार |
168 |
अगस्ति-पुल |
68 |
|
अगस्त्यकुंड |
76, 266, 268, 282, 297 |
अगस्त्येश्वर मंदिर |
268 |
|
आघा नूर |
245 |
अघोरास |
284 |
|
अघोरी शिव-शक्ति तांत्रिक साधनाएँ |
297 |
अघोरी टकिया |
157, 160, 260 |
|
अग्नि पुराण |
14, 29, 35, 166, 195, 203, 243, 268 |
अग्निश्वर घाट |
246, 289 |
|
कृषि का महत्व |
174 |
अहल्या बाई (इंदौर) |
252, 254-55, 268 |
|
अहल्या बाई घाट |
80, 251, 254, 293 |
अहिच्छत्र |
179, 209 |
|
आइया-के-बरह |
78 |
ऐल-पुरुरवा |
209-10 |
|
ऐतरेय ब्राह्मण |
21 |
अकबर |
229, 231-35, 240, 244-45, 294; शासनकाल 267; नीति 247, 284; समय 293 |
|
अब्दुल लतीफ |
233 |
अभिनवगुप्त |
110 |
|
आदमपुरा |
277 |
अधाई कंगूरे, मस्जिद |
215 |
|
अधाई-दिन-का-झोपड़ा |
215 |
आदि केशव |
35, 62, 122, 201, 205, 213, 218, 246, 294; केशवादित्य 58 |
|
आदि महादेव |
62 |
आदि शंकर |
192; सौंदर्य लहरी 162 |
|
आदि-विश्वनाथ पर्वत |
194 |
अफगानिस्तान, पठानों का अचानक आक्रमण |
284 |
|
मरणोत्तर संस्कार |
168 |
अगस्ति-पुल |
68 |
|
अगस्त्यकुंड |
76, 266, 268, 282, 297 |
अगस्त्येश्वर मंदिर |
268 |
|
आघा नूर |
245 |
अघोरास |
284 |
|
अघोरी शिव-शक्ति तांत्रिक साधनाएँ |
297 |
अघोरी टकिया |
157, 160, 260 |
|
अग्नि पुराण |
14, 29, 35, 166, 195, 203, 243, 268 |
अग्निश्वर घाट |
246, 289 |
|
कृषि का महत्व |
174 |
अहल्या बाई (इंदौर) |
252, 254-55, 268 |
|
अहल्या बाई घाट |
80, 251, 254, 293 |
अहिच्छत्र |
179, 209 |
|
आइया-के-बरह |
78 |
ऐल-पुरुरवा |
209-10 |
|
ऐतरेय ब्राह्मण |
21 |
अकबर |
229, 231-35, 240, 244-45, 294; शासनकाल 267; नीति 247, 284; समय 293 |
|
अक्षयवट मंदिर |
255 |
अल-बरूनी |
22, 29, 42, 45, 50, 203 |
|
अलाइपुरा |
191 |
आलमगिरी मस्जिद |
187, 248 |
|
अलाउद्दीन खिलजी |
217; देखें खिलजी |
अलीनगर |
286 |
|
अल्टेकर, "बनारस का इतिहास" |
60 |
अमरु |
110; उनके श्लोक 95 |
|
आभीर |
12 |
अवधगर्भी |
81 |
|
अमीर खुसरो |
110, 216 |
अमृत राव घाट |
293 |
|
आनंदकानन |
18, 28-31, 35-38, 41, 46-47, 50-51, 54, 57, 59-60, 70, 78, 80-81, 86-87, 90-97, 99-100, 111, 129, 164, 166, 172, 176-79, 187, 189, 191-93, 199, 202, 204-05, 207-10, 242, 268, 285-86, 297-98, 302-03; सुन्दर आश्रम 258; पूर्ववैदिक स्वरूप 201; आध्यात्मिक निवास 283; घाटी 273-74 |
अनंगपाल, सूर्य मंदिर |
215 |
|
पितृ-पूजा |
168 |
अंतरगृह |
117, 181, 259, 266 |
|
अंतरवेदी |
177 |
आपस्तंब गृह्यसूत्र |
22n |
|
अपोलो, पूजा |
58 |
आपटे, वी. एस., प्रैक्टिकल संस्कृत-अंग्रेज़ी शब्दकोश |
110 |
|
अर्दली बाजार |
285 |
अर्घ्य विनायक |
57 |
|
अर्क विनायक |
57 |
अस भैरव |
260-61 |
|
असी-संगम |
289; घाट 246 |
असितांग |
58 |
|
अशोक स्तंभ |
44 |
अष्टाध्यायी |
188 |
|
अश्वघोष |
39, 95, 102, 110 |
अश्वलायन गृह्यसूत्र |
22n, 167 |
|
अथर्ववेद |
22n, 67, 167-68, 173-74, 176 |
अत्रि |
11 |
|
औरंगाबाद चौकी |
266 |
औरंगजेब |
232, 247, 255, 262, 286, 296; शासनकाल 285 |
|
मूलनिवासी (ऑटोचथॉन्स) |
1, 2, 15, 19, 97, 158, 161, 169 |
अवंती |
179, 209 |
|
अविमुक्त मंदिर |
47, 51, 59, 66, 89, 190-91, 199 |
अविमुक्तेश्वर |
35, 122, 194, 200, 213; मंदिर 221, 235-37, 247, 255, 259, 277 |
|
बाबर |
224-25, 227-28 |
बड़ा गणेश |
278; मंदिर 260, 277 |
|
बद्रीनाथ |
300 |
बागेश्वरी |
86 |
|
बागिया माधोदास |
261 |
बहलोल लोदी |
227; देखें लोदी |
|
बैजाबाई (रानी), प्रयास |
296 |
बैजनाथ |
80 |
|
बैराम खान |
230 |
बाजीराव, पेशवा |
296 |
|
बल्लभी |
38 |
बलवंत सिंह |
250 |
|
बाणभट्ट |
22, 102; छंद 95 |
बनर्जी, आर. डी. |
33, 165 |
|
बकरियाकुंड |
35, 58, 70, 123, 200, 204, 220, 237, 248, 280, 282; मंदिर 44 |
बार्लो |
29 |
|
बाशम, ए. एल. |
165 |
बटुक भैरव |
160 |
|
बटुकनाथ |
78, 269 |
बौधायन श्रौतसूत्र |
21, 176 |
|
बेलघरिया (केनारामा-आस्थान) |
269 |
बेलवारिया |
78, 80 |
|
बंगाल, पाल वंश |
210 |
बंगालीटोला |
267, 297 |
|
बेनिया |
81, 191, 297 |
बेनिया बाग |
269 |
|
बेनियातालाब |
266, 276 |
बेनीमाधव मंदिर |
248 |
|
बर्नियर, फ्रांसिस |
42, 50, 249 |
भदैनी, लोलार्क |
58; देखें लोलार्क |
|
भद्रकाली |
82 |
भगवद्गीता |
168 |
|
भगवंदास |
229, 233-34 |
भैरव-शिव |
14 |
|
भैरव |
14-15, 42, 48, 53-54, 68, 77, 80 |
भैरवनाथ |
187 |
|
भंडास |
12, 19, 63 |
भरा-शैववाद |
35 |
|
भार/ भरा शिव |
19, 37, 48-49, 63-65, 212, 243, 285; पूर्व-आर्यन निवास 297; स्थानीय समुदाय 210 |
भार्गव |
10-11 |
|
भर्तहरि |
102, 110-11 |
भास |
102; छंद 95 |
|
भास्करानंद सरस्वती (स्वामी) |
180, 286n |
भानानारायण, नाटक |
69 |
|
भवभूति |
102; नाटक |
69 |
|
|
भवानी (अन्नपूर्णा) |
82, 115, 170, 213, 255; नया मंदिर |
भवानी/चंडी, प्रतिमा |
55 |
|
भीमाचंडी |
86 |
भीमाचंद विनायक |
57 |
|
भीषण |
58 |
भीतरी |
45-46, 48, 258, 287, 297 |
|
भोजू-बीर |
56, 81 |
भुवनेश्वर |
300 |
|
भुवनेश्वरी |
82 |
भूतही इमली |
261 |
|
भूतश्वर |
76, 255-56, 282, 297; तालाब 268; मंदिर 81 |
बिल्ल्हण, छंद |
95 |
|
बिंदुमाधव |
70, 199, 234; घाट 245, 289, 296; मस्जिद 260; मंदिर 249, 259, 285 |
बीर |
53-54, 68; मंदिर 49, 160 |
|
बीरबल |
229 |
बीरेश्वर घाट |
289, 296 |
|
बीरेश्वर मंदिर |
58; यमादित्य मंदिर |
बिसेसरगंज |
222, 261, 277 |
|
ब्लोफील्ड, जॉन, आई-चिंग |
105, 107 |
बोधगया |
38 |
|
बोनार |
31 |
ब्रह्म घाट |
244-45, 289 |
|
ब्रह्मनाला |
282 |
ब्राह्मणीय आर्यत्व |
158 |
|
ब्रह्म पुराण |
21 |
ब्रह्मसरोवर |
76, 269, 282 |
|
ब्रह्मवैवर्त पुराण |
168 |
बृद्धादित्य घाट |
289 |
|
बृद्धकला |
277 |
बृहदारण्यक उपनिषद |
21, 22n, 176 |
|
बुद्धादित्य घाट |
246 |
बौद्धघोष |
69-70 |
|
बुद्ध का इसिपत्तन |
60-62; देखें इसिपत्तन |
बौद्ध धर्म, वज्रयान रूप |
39 |
|
बुलानाला |
189; तालाब 261 |
बुढ़वा-मंगल, सांस्कृतिक गतिविधि |
289n |
|
चामुंडा |
56 |
चंड |
58 |
|
चंद्रदेव, कन्नौज के राजा |
70 |
चरक |
39 |
|
जाति प्रथा |
13, 65 |
चतुःषष्टि योगिनी / चौसठी घाट |
76, 80, 82, 245, 267, 289, 290, 293-94 |
|
चौहान, पृथ्वीराज |
214 |
छांदोग्य उपनिषद |
22, 174 |
|
चंद्रवार, युद्ध |
214 |
चेतसिंह (राजा) |
28, 279; सचिव 44 |
|
चेतसिंह किला |
81, 112, 292 |
चौकी घाट |
261, 293-94 |
|
चिंतामणि विनायक |
57 |
क्लाइव |
29, 263 |
|
समुदाय, धार्मिक भावना |
226 |
धर्म परिवर्तन |
191, 271-73 |
|
कुमारस्वामी, आनंद के. |
40 |
ब्रह्मांडीय नाभि, रहस्यमय अवधारणा |
93 |
|
कनिंघम |
44 |
कर्जन, लॉर्ड |
276 |
|
दक्षिण कालीका |
106 |
डलहौजी |
263 |
|
दलमंडी |
191, 222 |
दलपत राय घाट |
251, 296 |
|
डंडपाणि, गणेश मंदिर |
14, 160 |
डंडपाणि भैरव |
255 |
|
डंडेश्वर विनायक |
57 |
दंठहस्त-गणेश्वर (बड़ा गणेश) |
35, 237 |
|
दंतवक्त्र |
67 |
दांते |
110 |
|
दरानगर |
286 |
दारा शिकोह |
247, 285 |
|
दरभंगा, महाराजा |
80; भवन निर्माण 293 |
दशाश्वमेध घाट |
53, 65, 76, 189, 199, 243, 246, 266-67, 289-90, 294 |
|
दत्तात्रेय |
111, 113; घाट 114, 296; मंदिर 295 |
दयानंद |
184 |
|
देहाती विनायक |
57 |
देवरिया-बीर |
56, 81 |
|
देव |
49 |
डेरसी (देउरी-शिव) का पुल |
68 |
|
देव-गण संघर्ष |
160 |
देवनाथपुरा, मुस्लिम बस्तियों का विस्तार |
285 |
|
एकदंता |
14 |
इलियट, रॉबर्ट (कैप्टन) |
251 |
|
अंग्रेजी प्रशासन, नगर योजना |
29 |
फा-हिएन |
22, 29, 50, 55, 83, 179, 184, 205 |
|
फैज़ी, अबुल फज़ल |
229 |
सामंतवाद, संघर्ष |
227 |
|
फिराक |
110 |
फिरोज शाह तुगलक |
124, 220, 222, 231-32 |
|
फिट्च, राल्फ |
50, 244, 288 |
फ्लीट, जे.एफ., गुप्त शिलालेख |
65n |
|
फ्लेचर, सर रॉबर्ट |
9 |
जबरन धर्मांतरण की समस्या |
24 |
|
गदुरेश्वर |
183 |
गहड़वाल |
31, 36-37, 55-56, 63, 158, 210, 213-15, 219, 244, 246, 283-84 |
|
गहना बाई, दानशीलता |
296 |
गैवी |
78, 80, 82 |
|
गजतुंड |
57 |
गण-भूत, आदिवासी पूर्व-धारणा |
168 |
|
गण-देवता, पशु-मुखी |
12 |
गणपति |
53-54 |
|
गण |
31, 49-50, 53, 68, 242-43 |
गण-शिव और विष्णु युद्ध |
38 |
|
गांधार |
40 |
गंधर्व |
50 |
|
गणेश |
12, 14, 49, 53 |
गणेश चौथा |
86 |
|
गणेश मोहल्ला |
81, 267 |
गंगा-केशव |
289 |
|
गंगा महल घाट |
293, 296 |
गरुड़ पुराण |
168 |
|
गौरीपीठ/ गौरीपीठम |
18, 36, 47, 51, 55, 59, 66, 98-99, 172, 191, 199, 201, 210, 286, 297 |
गौतम बुद्ध |
184, 257, 283 |
|
गौतम धर्मसूत्र |
22n |
गावस्ती, पूजन |
58 |
|
गया घाट |
289 |
गाजीपुर |
23, 45-46, 188, 258 |
|
ग़ालिब |
110 |
घंटाकर्ण |
86 |
|
घोड़ा घाट |
244-45, 280 |
घोड़ा-शिव, प्राचीन आर्य पूर्ववास |
297 |
|
घोरी, सेनाएँ |
36 |
ग़ुलाम कादिर |
244 |
|
गोदावरी नाला |
285 |
गोदावरी तीर्थ |
282 |
|
गोदौलिया |
117, 189, 266, 290, 297 |
गोएथे |
110 |
|
गोकर्णेश्वर |
67 |
गोला- दीनानाथ |
261 |
|
गोमती संगम, निकट बस्ती |
287 |
गोपाल |
82 |
|
गोपथ ब्राह्मण |
21, 176 |
गोप्रेक्षा विनायक |
57 |
|
गोरखनाथ |
184 |
गोरखनाथ टीला |
260-62 |
|
गोरकटीला |
86, 237 |
गोवर्धन, प्रसिद्ध टोडरमल के पुत्र |
38 |
|
गोविंदचंद्र |
38, 278 |
ग्रेको-स्किथियन रूप |
170, 177 |
|
महान धामेक स्तूप |
46 |
महान हिंदू-संगम |
224 |
|
गुह्यक |
50, 243 |
गुप्त |
210 |
|
गुरनपुर/ गुरुपुर |
43 |
हैहय |
31, 32 |
|
हैहय-कालचुरी |
14 |
हनुमान घाट |
292 |
|
हनुमंता, महावीर |
14 |
हड़प्पा, मिट्टी के निर्माणकर्ता |
10 |
|
हड़प्पा संस्कृति |
13, 48, 158, 161 |
हरिश्चंद्रेश्वर, एक मंदिर |
199 |
|
हरिश्चंद्र घाट |
112-14, 292-93 |
हर्ष |
210 |
|
हस्ति विनायक |
57 |
हेस्टिंग्स, वॉरेन |
29, 85, 263, 276, 279 |
|
हेमचंद्र (राजा) / (हेमू) |
230 |
हेनोथिज्म, मूल विचार |
223 |
|
हिंदू-बौद्ध केंद्र, समय-समय पर लूट |
39 |
हिंदू-मुस्लिम भेदभाव और विवाद |
281 |
|
हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र |
67 |
ऐतिहासिक प्रक्रिया की जटिलता |
30 |
|
ह्वेनसांग |
22, 29, 32, 45, 50, 55, 83, 121, 123, 165, 179, 184, 192, 200, 203, 205, 208, 212 |
होयसल |
217 |
|
हुमायूँ |
38, 224, 227-30 |
इब्न बतूता |
42, 50, 203 |
|
इब्राहिम लोदी |
225, 227 |
इल्तुतमिश |
124, 217, 231-32 |
|
इम्पी |
29 |
इंडियन एंटीक्वेरी |
213n |
|
इंदौर, होलकर |
80 |
अंतर्सामुदायिक समझ |
217 |
|
आंतरिक राजनीतिक संघर्ष |
284 |
इकबाल |
110 |
|
इसरगंगी |
183, 204, 220, 222, 256, 266 |
तालाओ |
186 |
|
इसिपत्तन/ ऋषिपत्तन |
22 |
इस्लामी कट्टरवाद |
223 |
|
जगद्धात्री |
82 |
जगतगंज |
222, 261, 265 |
|
जगत सिंह |
44 |
जहान्दार शाह |
244-45, 286 |
|
जहांगीर |
245, 267, 247, 284 |
जयचंद्र, गहड़वाल राजा |
35 |
|
जैन-बौद्ध युग, अव्यवस्था |
65-66 |
जय सिंह |
291 |
|
जैतपुरा |
191, 222, 277 |
जलालपुरा |
277 |
|
जलालुद्दीन रूमी |
110 |
जलंधरनाथ (नाथ योगी) |
237 |
|
जलसयी घाट |
295-96 |
जलेश्वर घाट |
113 |
|
जमदग्नि |
111 |
जमालपुरा/ जमालुद्दीनपुरा |
214 |
|
जमालुद्दीन |
214 |
जाम घाट (यम घाट) |
295 |
|
जनस्थान, विनाश |
13 |
जरासंध घाट |
246, 289, 294 |
|
जातक |
22, 29, 176, 192 |
जतांबर |
222, 259 |
|
जौनपुर, लाल दरवाजा मस्जिद |
218 |
शर्की शासक |
36, 124, 127 |
|
जया |
11, 13 |
जयंत |
57 |
|
झूंसी में गंगेयदेव का शिलालेख |
213n |
जिनप्रभा सूरी, विविध तीर्थकल्प |
191, 195, 219-20 |
|
जितवारी |
188, 205 |
ज्ञानवापी |
70, 100, 117-18, 123, 127-29, 200, 207, 213-14, 218, 290, 301 |
|
जोन्स, सर विलियम |
276 |
कबीर |
184 |
|
कबीर चौरा |
189, 265 |
कबीर दास (संत), उत्पीड़न |
261 |
|
कैकोबाद (सुल्तान) |
216-17, 232 |
काल भैरव |
4, 14, 160, 214, 237 |
|
कालचुरी |
36 |
गंगेयदेव |
213 |
|
कालमुख |
80 |
काला पहाड़ |
272, 285 |
|
कलेश्वर मंदिर |
190 |
कल्हण |
39, 95 |
|
कल्हुआ |
82 |
काली |
82, 295 |
|
कालीबंगा, मिट्टी के निर्माणकर्ता |
10 |
कालिदास |
102, 110, 95 |
|
काली महल |
285 |
कालिका |
77 |
|
काल-माँ |
260 |
कालवी |
105 |
|
कामच्छा |
78, 82 |
कामेश्वर, खाखोलादित्य |
58 |
|
किरात |
50 |
कोल्हुआ |
80 |
|
कोना विनायक |
57 |
कोसला |
22, 210 |
|
कौशाम्बी |
179, 209 |
कौशीतकी |
176 |
|
कौटिल्य |
102 |
अर्थशास्त्र |
22 |
|
कविराज, गोपीनाथ |
18 |
केदार |
267, 283 |
|
केदार घाट |
80, 112, 241, 246, 280, 289-90, 292-94 |
केदारखंड |
59, 70, 112, 180, 186, 293 |
|
केदारनाथ |
300 |
केदारेश्वर |
300 |
|
केनाराम, अघोरी |
180, 292 |
आश्रम |
81, 269 |
|
केशव मंदिर |
292 |
खालिशपुरा, मुस्लिम बस्तियाँ |
285 |
|
खरवेला |
38 |
खरपरसी |
48 |
|
खरवा विनायक |
57, 62 |
खिल महाभारत |
115 |
|
खिलजी |
39, 124-26, 215, 219 |
खोजवाह |
56, 78, 80, 220 |
|
खोजवाह तालाओ |
204 |
किल्टो (मेजर) |
44 |
|
लक्ष्मी चबूतरा |
283, 290 |
लक्ष्मी घाट |
293 |
|
लक्ष्मीकुंड |
204, 297 |
ललिता |
115, 170 |
|
ललिता घाट |
294 |
ललितास्तक-रत्नम |
162 |
|
ललितासुंदरी |
76 |
लक्ष्मिधर, क्रिया कल्पतरु |
56, 200, 258, 268, 278 |
|
तीर्थ विवेचनखंड |
35, 56, 200, 213n |
लाली घाट |
293 |
|
लाट |
49, 53 |
लाट भैरव |
220, 277 |
|
लौरिया-बीर |
56 |
ल्हादिनी |
115 |
|
जीवन-मरण, वैदिक दृष्टिकोण |
167 |
जीवन-प्रक्रिया, रहस्यमय क्षेत्र |
171 |
|
जीवन-शक्ति की आराधना |
95 |
लिंग पुराण |
65, 187, 200 |
|
लिंगम और पल्ली, विचार |
171 |
लोदी |
39, 124 |
|
लोलार्क |
266, 289 |
लोलार्क घाट |
246, 289 |
|
लोलार्क कुंड |
86, 292 |
सूर्य देवता |
81 |
|
तालाब |
256 |
मंदिर |
246 |
|
लंदन बौद्ध सोसाइटी, अध्यक्ष |
107 |
लुक्सा चौकी |
266 |
|
चंद्र वंश, शासक |
209 |
माँ आनंदमयी |
180, 184 |
|
माँ आनंदमयी घाट |
245, 292 |
मच्छोदरी |
85, 122, 158, 187, 200, 236, 278-80, 282 |
|
मच्छोदरी नाला |
259, 280 |
मच्छोदरी झील |
289, 297 |
|
माछोदरी चैनल |
261, 268 |
मिट्टी का किला |
65 |
|
मैसिडोनियन प्रवेश |
40 |
मैकेंज़ी (कर्नल) |
44, 46 |
|
मदन चंद |
219 |
मदनपुरा |
191, 297 |
|
मुस्लिम बस्तियाँ |
285 |
मदन वाराणसी/ जमनिया |
219 |
|
माधोदास की बगिया |
276, 279 |
माधुसूदन सरस्वती (स्वामी) |
286n |
|
मध्येश्वर |
122, 187, 190, 194, 199, 277 |
मंदिर |
213, 248, 278 |
|
वाराणसी मंदिर |
214 |
माध्यमिक या कुषावर्त |
19 |
|
मदोत्कट |
57 |
महाभारत |
9-12, 22, 29, 41, 161, 166, 184, 258 |
|
महादजी सिंधिया |
291 |
महाकाल |
199 |
|
मंदिर |
213, 248, 259 |
वाराणसी मंदिर |
214 |
|
महाकालेश्वर |
122, 194, 300 |
मंदिर |
235 |
|
महामायूरी जर्नल |
64 |
महाजनचोला |
222 |
|
महाराजा विनायक |
57 |
महास्मशान |
18, 20, 36, 37, 47-49, 55, 66-67, 78, 99, 111-14, 119, 168, 170-72, 192, 201, 242, 258, 286, 301-02 |
|
महावीर (वर्धमान) |
184 |
महायान तंत्र |
103 |
|
महेश्वर |
80 |
महेश्वर-कापालिक |
158 |
|
माहिष्मती |
179 |
महमूद ग़ज़नी |
24, 31, 173, 211, 213, 214 |
|
सेनाएँ |
36 |
मैदागिन |
260, 277, 290 |
|
मलिक काफूर |
217, 285 |
मम्मट |
110 |
|
मृगदाव-सारनाथ |
22-23 |
मुद्गरपाणि |
57 |
|
मुग़ल |
124, 224 |
मुंशी घाट |
80, 250, 293 |
|
मणिकर्णीश्वर मंदिर |
218 |
मनमंदिर घाट |
76, 80, 294 |
|
मंसा राम |
250 |
मान सिंह (राजा) |
229, 240, 246, 290-91, 293 |
|
मनु |
11 |
मनुस्मृति |
22, 117 |
|
मराठा |
244, 250 |
वर्चस्व |
252 |
|
मारीचि |
33 |
मार्कंडेय |
45, 111, 188 |
|
मार्कंडेय पुराण |
166 |
मार्शल, सर जॉन |
44, 165 |
|
मातंगी, मंदिर |
295 |
मातृकुंड |
165 |
|
मत्स्य पुराण |
14, 53-54, 200, 243, 268 |
मत्स्योदरी |
36, 186 |
|
मौर्य |
210 |
मेगास्थनीज |
22 |
|
मेसोपोटामियन और ईरानी सामाजिक रूप |
40 |
मियां तानसेन |
233 |
|
मिहिर, पूजा |
58 |
मीर घाट |
199, 250, 294 |
|
बृध्दादित्य |
58 |
मिसिर पोखरा |
165, 186, 189 |
|
मोड़ा विनायक |
57 |
मुहम्मद ग़ोरी |
22, 214 |
|
मुहम्मद शर्की |
220, 232, 286 |
मुहम्मद तुगलक |
191, 219, 231-32 |
|
मोक्षद्वार प्रवेश |
246, 289 |
मोक्ष लक्ष्मी विलास मंदिर |
121, 123, 127-28 |
|
मोतीचंद्र |
200 |
काशी का इतिहास |
187 |
|
मृगदाव |
36, 69, 188, 209, 257, 259, 283 |
मंदिर का विनाश |
213 |
|
नाग |
19, 48, 50, 80 |
नागार्जुन |
50 |
|
नागेश्वर घाट/ भोंसला घाट |
245-46, 289 |
नग्निकास |
33 |
|
नागपंचमी |
86 |
नक्कटैया |
86 |
|
नालंदा |
30, 38, 209 |
नामदेव |
105 |
|
नंद कुमार (राजा) |
279 |
नंद घाट |
280 |
|
नंदिकेश |
14 |
नंदिकेश्वर |
67 |
|
नराकार (न-क्रोध या अक्रोध)/ सारंगताल |
43 |
नारायण भट्ट, तीर्थ कल्पतरु |
195, 230 |
|
नारायण दीक्षित, पंडित |
244, 250-52 |
नारायण दत्त, पंडित |
234-38, 255, 285 |
|
नारियलटोला |
222 |
नाते इमली |
222, 261, 265 |
|
नाथ-अघोरी, प्राचीन आर्य पूर्व संप्रदाय |
260 |
नाथद्वारा, पल्लव |
105 |
|
प्राकृतिकवाद |
223 |
नयाताल |
43 |
|
नेपाली-खपरा घाट |
295 |
नियालटगिन |
212-13 |
|
निकुंभ |
31 |
निकुंभेश्वर |
67 |
|
निनेवेह |
30 |
निर्ग्रंथ |
33, 48, 50 |
|
निज़ामुद्दीन औलिया, हजरत |
216 |
ओर्टेल |
44 |
|
ओंकार |
199 |
ओंकार मंदिर |
190, 213, 247, 259, 278 |
|
ओंकारखंड |
39, 57, 59, 70, 80, 83, 86, 180, 186-87, 207, 297 |
ओंकारेश्वर |
35, 122, 194, 303-04 |
|
ओविड |
110 |
पुष्टि और मर्यादा, वल्लभ का विचार |
106 |
|
पुष्यमित्र (सुंग) |
38 |
पंचबाग्गीय शिष्य |
61 |
|
पद्मेश्वर मंदिर |
218, 221 |
पैप्पलाद संहिता |
21 |
|
पैशाचिक संस्कार |
32 |
पक्की महल |
222, 259, 289 |
|
पक्की मोहल्ला |
206 |
पालत्रिय, विशेष प्रकार के |
11 |
|
पंचगंगा घाट |
70, 80, 100, 201, 243, 283-84, 289 |
बिंदुमाधव मंदिर |
296 |
|
पंचक्रोशी, परिक्रमा |
180-81 |
पांडेय घाट |
245, 293 |
|
पंढरपुर, दास |
105 |
पांड्य |
217 |
|
पाणिनि |
39 |
पंथ लेख |
55-56 |
|
परशुराम |
111 |
पर्रे घाट |
80 |
|
पार्थियन उपनिवेश |
40 |
पाशपाणि विनायक |
57 |
|
पाशुपत |
67 |
पाशुपति, संप्रदाय |
161, 165 |
|
पशुपतिनाथ |
300 |
पातालेश्वर |
76 |
|
पतंजलि |
50, 205 |
महाभाष्य |
176 |
|
पठान, हिंदू नीति |
231 |
पठान ग़ोरी (ग़ुलाम वंश) |
124 |
|
पेशवा घाट/ बालाजी घाट |
251, 296 |
पिशाचमोचन |
81, 86, 160, 165, 204, 261, 266, 282 |
|
तालाब |
186 |
टैंक |
250 |
|
पीरकुंडा |
35, 165, 280 |
मंदिर |
44 |
|
बहुदेववाद |
223 |
पोटली |
188 |
|
प्रबंधकोश |
217 |
प्रद्योत, काल |
38 |
|
प्रज्ञापारमिता |
103 |
प्रतापादित्य |
76, 267, 286 |
|
प्रतिहार |
14, 32, 36 |
प्रतिष्ठान |
209 |
|
प्रयाग घाट |
189, 199, 246, 294 |
प्रयाग घाट-कम-घोड़ा घाट |
282 |
|
प्रेत-कृत्य |
167-68 |
आदि माता-पिता संयोग |
66 |
|
प्रिंसेप, सर जेम्स |
9, 31, 251, 260, 276, 295 |
पुल-की-काली |
68 |
|
पुरुष-प्रकृति संयोग |
20 |
पुरुषपुर |
209 |
|
महमूद की जयपाल पर विजय |
212 |
पुष्पदंत |
14, 160 |
|
मंदिर |
267 |
कुतुबुद्दीन ऐबक |
22, 124, 214-15 |
|
राजबल्लभ घाट |
113 |
राजधानी वाराणसी |
219 |
|
राजा घाट |
80, 293-94 |
राजराजेश्वरी |
82 |
|
राजस्थान, राजपूत घराने |
287 |
राजघाट |
245, 289 |
|
अनोखी मस्जिद (राजघाट) |
215 |
किला (राजघाट) |
70, 82, 244 |
|
राजघाट थियोसोफिकल कॉलेज |
37 |
राजगीर |
38 |
|
राक्षस |
20, 50 |
राम घाट |
246, 289, 296 |
|
रामकृष्ण परमहंस |
180, 184 |
रामलीला |
86 |
|
रामनगर |
242 |
किला (रामनगर) |
294 |
|
रामानंद |
184 |
रामायण |
184 |
|
रामेश्वर घाट |
246, 289 |
राणा घाट |
251 |
|
राणा महल घाट |
293-94 |
रानी भवानी (नटोर) |
82, 252-55, 268, 278, 286 |
|
रणजीत सिंह, महाराजा (पंजाब) |
255 |
राष्ट्रकूट |
210 |
|
रजिया मस्जिद |
222, 236 |
रजिया सुल्ताना |
217, 232 |
|
रजिया बेगम की मस्जिद |
123, 127 |
पुनर्जन्म अवधारणा |
167-68 |
|
रेओरीतालाओ/ रेवतीतालाब |
80-81, 90, 165, 204, 265-66, 282 |
पुनरुत्थान (यहूदी/ईसाई) |
111 |
|
रेवतीकुंड |
78-79, 186, 204, 297 |
ऋग्वेद |
20-21, 173 |
|
ऋणमोचन |
278, 280, 282 |
रुद्र पशुपति, अनुयायी |
50 |
|
रुद्रसरोवर |
256, 268, 294 |
रुद्रवास |
18, 20, 29-30, 36-38, 40-41, 47, 50, 54, 59, 64, 66-67, 70, 99, 176-78, 181-82, 184, 191-92, 201, 269, 286, 294, 298, 302 |
|
भारा-शैव (रुद्रवास) |
32 |
रुद्रीय |
31 |
|
रुरु |
58 |
रुरु भैरव, मंदिर |
292 |
|
रुस्तम अली, मीर |
250, 289n, 294 |
सावाचार |
158 |
|
सवाई जयसिंह |
76 |
सिंधिया घाट |
245, 296 |
|
यौन-प्रेरणा |
102-03 |
शाह आलम |
286 |
|
शाह आलम द्वितीय |
244 |
शाहजहां |
247 |
|
शेक्सपीयर |
110 |
शार्की |
220 |
|
शेर शाह |
38, 228-29 |
शिवाजी |
248 |
|
श्रीनगर, बड़ी मस्जिद |
262 |
सिद्ध |
50 |
|
सिद्ध विनायक घाट |
246, 289 |
सिद्धेश्वरी घाट |
280 |
|
सिद्धि विनायक |
57 |
सिगरा-रथ-तल्ला |
82 |
|
सिकंदर लोदी |
124, 222, 227, 235, 296 |
सिंदूर विनायक |
57 |
|
शीतला घाट |
294 |
शिव, त्रिआयामी प्रतिमा |
211-12 |
|
शिव-भैरव संप्रदाय |
97 |
शिवाचार |
158 |
|
शिव संस्कृति |
3, 54 |
शिव-क्षेत्र/ रुद्रवास |
98 |
|
शिवाला घाट |
292 |
शिव-पशुपति देवता |
212 |
|
शिव पुराण |
243 |
शिव-शक्ति भैरव (वाम) पूजा |
295 |
|
शिव-विश्वेश्वर |
115 |
शिव-यक्ष |
35 |
|
स्कंद पुराण |
14, 21, 187, 300 |
श्मशान-विनायक मंदिर |
199 |
|
मंदिर |
295 |
सामाजिक परिवर्तन |
117 |
|
सोडेपुर |
45-46, 48, 60, 287 |
सोडेपुर-भीटरी-कपिलधारा क्षेत्र |
288 |
|
सोलोनो |
86 |
सोमनाथ |
300 |
|
सोमेश्वर |
170 |
सोमेश्वर घाट |
246, 289, 298 |
|
स्पंद' |
110 |
अज्ञात आत्मा का मंदिर |
160 |
|
श्रावस्ती |
209 |
श्रीधर प्रसाद, मुंशी |
293 |
|
सृष्टि विनायक |
57 |
सदानीरा (गंडकी) |
20 |
|
सादी |
110 |
सहरबाग |
261 |
|
सईदपुर |
188 |
शैव संस्कार, केंद्र |
12 |
|
शैव-शक्ति-जैन-बौद्ध-वैष्णव संघर्ष |
38 |
शैव गतिविधियाँ |
35 |
|
साक्षी विनायक |
57 |
साक्षी विनायक मंदिर |
160 |
|
शक्ति, तांत्रिक संप्रदाय |
210 |
संभर्ता |
111 |
|
संहारा |
58 |
समुद्रगुप्त |
38 |
|
शंकराचार्य |
184 |
शंकरमठ |
82, 187 |
|
शंकरनाथ |
80 |
संकट घाट |
80, 296 |
|
संकटमोचन |
80, 187 |
सांख्यायन श्रौतसूत्र |
21, 176 |
|
संखोधारा |
81 |
संतरास' |
242 |
|
सापमोचन |
278, 280 |
सफो |
110 |
|
सारनाथ |
31, 188, 257, 283, 287, 297 |
सरंगनाथ |
257 |
|
सरंगेश्वर |
43 |
सर्वेश्वर घाट |
246, 289 |
|
ससांक (बंगाल) |
38 |
शास्ता |
33 |
|
सालपथा ब्राह्मण |
20-21, 22n, 53, 176, 190 |
सातवाहन |
31, 33 |
|
सत्यनारायण मंदिर |
218 |
सौराष्ट्र, सोमनाथ |
190 |
|
स्टाइन, ऑरेल |
165 |
स्थानु, आधार |
171 |
|
पत्थर युग संस्कृति |
11 |
सूद्रक |
102 |
|
सुयर्स |
10 |
शुक्रेश्वर |
170 |
|
सुलह-ए-कुल (सार्वभौमिक सहिष्णुता नीति) |
233 |
सुलपाणि |
57 |
|
सुलतानकेश्वर, भूमिगत मंदिर |
76 |
सूर्य, पूजा |
58, 86 |
|
सुंग |
33, 38, 210 |
सूरजकुंड |
204, 256, 266, 282 |
|
संबादित्य |
58 |
सुश्रुत |
39 |
|
स्वप्नेश्वर मंदिर |
246 |
स्वर्गद्वार प्रवेश/ मणिकर्णिका |
246, 289 |
|
स्वयंभू |
194 |
स्वयंभू लिंग |
190, 299-300 |
|
रवींद्रनाथ टैगोर |
109 |
तैलंग स्वामी |
180 |
|
तैत्तिरीय आरण्यक |
22n |
तक्षशिला |
30, 209 |
|
ताम्रलिप्ति, वर्गभीम मंदिर |
43 |
तंत्र/ तांत्रिक संप्रदाय |
81, 97 |
|
तंत्र-यक्ष |
35 |
तांत्रिक भैरव संप्रदाय |
48 |
|
तारा |
82 |
देवी की छवियाँ |
36 |
|
टैवर्नियर, जीन फ्रांसिस |
42, 50, 203, 249, 296 |
मंदिर विध्वंस, तथ्य |
271 |
|
तेरी नीम |
78 |
तराइन, दूसरा युद्ध |
214 |
|
ठाकुर सीताराम ओंकारनाथ, अवधूत |
180, 290 |
थानेश्वर, शासक |
210 |
|
तित्तिर |
11 |
टोडरमल |
229, 233-34, 240, 288 |
|
त्रिलोचन |
189, 222, 303-04 |
अरुणादित्य (त्रिलोचन) |
58 |
|
त्रिलोचन घाट |
244, 246, 289 |
त्रिलोचन मंदिर |
246, 259 |
|
त्रिपुरा या ललिता, मंदिर |
295 |
त्रिपुरा भैरवी घाट |
294 |
|
त्रिपुरा सुंदरी |
295 |
त्रिपुरेश्वरी |
76, 170 |
|
तुगलक |
39, 124, 219 |
अमीर खुसरो |
110, 216 |
|
अमृत राव घाट |
293 |
आनंदकानन |
18, 28-31, 35-38, 41, 46-47, 50-51, 54, 57, 59-60, 70, 78, 80-81, 86-87, 90-97, 99-100, 111, 129, 164, 166, 172, 176-79, 187, 189, 191-93, 199, 202, 204-05, 207-10, 242, 268, 285-86, 297-98, 302-03 |
|
अनंगपाल, सूर्य मंदिर |
215 |
पूर्वज पूजा |
168 |
|
अंतरगृह |
117, 181, 259, 266 |
अंतरवेदि |
177 |
|
आपस्तंब गृह्यसूत्र |
22n |
अपोलो, पूजा |
58 |
|
आप्टे, वी.एस., संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश |
110 |
अर्दली बाजार |
285 |
|
अर्घ्य विनायक |
57 |
अर्क विनायक |
57 |
|
अस भैरव |
260-61 |
असि-संगम |
289; घाट 246 |
|
असितांग |
58 |
अशोक स्तंभ |
44 |
|
अष्टाध्यायी |
188 |
अश्वघोष |
39, 95, 102, 110 |
|
अश्वलायन गृह्यसूत्र |
22n, 167 |
अथर्ववेद |
22n, 67, 167-68, 173-74, 176 |
|
अत्रि |
11 |
औरंगाबाद चौकी |
266 |
|
औरंगजेब |
232, 247, 255, 262, 286, 296 |
उनके शासनकाल में |
285 |
|
आदिवासी |
1, 2, 15, 19, 97, 158, 161, 169 |
अवंति |
179, 209 |
|
अविमुक्त मंदिर |
47, 51, 59, 66, 89, 190-91, 199 |
अविमुक्तेश्वर |
35, 122, 194, 200, 213 |
|
अविमुक्तेश्वर मंदिर |
221, 235-37, 247, 255, 259, 277 |
भार्गव |
10-11 |
|
भर्तृहरि |
102, 110-11 |
भास |
102; श्लोक |
|
भास्करानंद सरस्वती (स्वामी) |
180, 286n |
भानानारायण, नाटक |
69 |
|
भवभूति |
102; नाटक |
69 |
भवानी (अन्नपूर्णा), नया मंदिर |
|
भवानी/ चंडी, मूर्ति |
55 |
भीमाचंडी |
86 |
|
भीमचंद विनायक |
57 |
भीषण |
58 |
|
भीटरी |
45-46, 48, 258, 287, 297 |
भोजू-बीर |
56, 81 |
|
भुवनेश्वर |
300 |
भुवनेश्वरी |
82 |
|
भूतही इमली |
261 |
भूतश्वर |
76, 255-56, 282, 297 |
|
भूतश्वर तालाब |
268 |
भूतश्वर मंदिर |
81 |
|
बिल्हण, श्लोक |
95 |
बिंदुमाधव |
70, 199, 234 |
|
बिंदुमाधव घाट |
245, 289, 296 |
बिंदुमाधव मस्जिद |
260 |
|
बिंदुमाधव मंदिर |
249, 259, 285 |
बीर |
53-54, 68 |
|
बीर मंदिर |
49, 160 |
बीरबल |
229 |
|
बीरेश्वर घाट |
289, 296 |
बीरेश्वर मंदिर, यमादित्य |
58 |
|
बिसेस्सरगंज |
222, 261, 277 |
ब्लोफील्ड, जॉन, आई चिंग |
105, 107 |
|
बोधगया |
38 |
बोनार |
31 |
|
ब्रह्म घाट |
244-45, 289 |
ब्राह्मणाला |
282 |
|
ब्राह्मणीय आर्य संस्कृति |
158 |
ब्रह्म पुराण |
21 |
|
ब्रह्मसरोवर |
76, 269, 282 |
ब्रह्मवैवर्त पुराण |
168 |
|
वृद्धादित्य घाट |
289 |
वृद्धकाल |
277 |
|
बृहदारण्यक उपनिषद |
21, 22n, 176 |
बुद्धादित्य घाट |
246 |
|
बुद्धघोष |
69–70 |
बुद्ध के ईसिपत्तन |
60-62 |
|
बौद्ध धर्म, वज्रयान संप्रदाय |
39 |
बुलानाला |
189; तालाब 261 |
|
बुड़वा-मंगल, सांस्कृतिक गतिविधि |
289n |
चक्रतीर्थ |
201; कथा 100-101-111 |
|
देव वाराणसी |
219 |
देवी भागवत |
115 |
|
धम्मपद अलकथा |
22 |
धारावती |
209 |
|
धृतराष्ट्र |
38 |
ध्रुवेश्वर |
170, 297 |
|
धुंडी विनायक |
57 |
धुंडीराज |
255 |
|
दिवोदास, समय |
38 |
डफ़रिन ब्रिज (अब मालवीय ब्रिज), निर्माण |
280 |
|
दुर्गा घाट |
244-45, 289 |
दुर्गाकुंड |
256 |
|
दुर्गा विनायक |
57 |
डटन, तांत्रिक रहस्यवाद |
106n |
|
द्वारका |
179 |
एकदंत |
14 |
|
इलियट, रॉबर्ट (कप्तान) |
251 |
अंग्रेजी प्रशासन, नगर योजना |
29 |
,