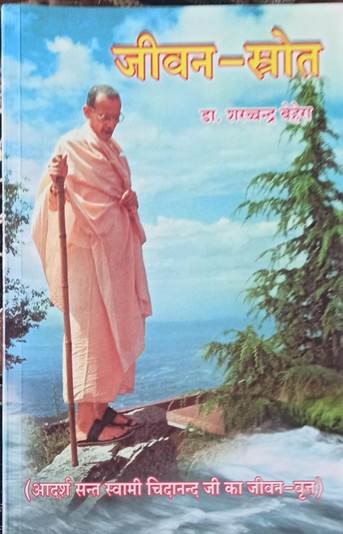
जीवन-स्रोत
आदर्श सन्त स्वामी चिदानन्द के विशद जीवन-वृत्त
THE HOLY STREAM
का हिन्दी भाषान्तर
लेखक
डा. शरच्चन्द्र बेहेरा, एम.ए., पी-एच.डी.
अनुवादक
श्री स्वामी अर्पणानन्द सरस्वती
(पूर्वाश्रम-नाम श्री चमनलाल शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल)
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण - १९८४
द्वितीय हिन्दी संस्करण-२००७
तृतीय हिन्दी संस्करण-२०१६
(५०० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
HO23
PRICE: 150/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए
स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त फारेस्ट
एकाडेमी प्रेस, शिवानन्दनगर- २४९१९१२, टिहरी-गढ़वाल,
उत्तराखण्ड' में मुद्रित ।
For online orders and Catalogue visit: dlsbooks.org

परम पूज्य श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज

परम पूज्य स्वामी जी के साथ लेखक
प्रकाशकीय
यह पुस्तक पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज का जीवन-वृत्त है। काल-सिकता पर पड़े उनके चरण-चिह्न अमिट हैं। उनका जीवन लौकिकता तथा अलौकिकता दोनों का ही एक अद्भुत संगम है। वह लौकिक हैं, क्योंकि वह लोक-हित में सतत रत हैं। वह अलौकिक हैं, क्योंकि वह अलौकिक दिव्यता के धनी हैं। उनका जीवन सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज की अनुकृति ही है। परम पूज्य सद्गुरुदेव ईश्वरोन्मुख उन्नत शिर तथा धरती पर रखे हुए पैरों वाले भगवत्पुरुष थे। उनके विषय में दिये गये इस वक्तव्य की जीवन्त व्याख्या है पूज्य स्वामी चिदानन्द जी महाराज का जीवन।
पूज्य स्वामी जी एक-साथ ही सब-कुछ हैं-भागवती चेतना में संस्थित महापुरुष, असाधारण शिष्य, मानवता के सेवक, सन्त-प्रेमी, आध्यात्मिक सम्पदा के वितरक तथा महान् प्रबोधक। ऐसे महापुरुष की जीवन-गाथा प्रस्तुत करके हम गौरवान्वित हुए हैं। कभी उन्होंने कहा था- "इस जीवन का अस्वीकरण नहीं करें, इसका रूपान्तरण करें।" आशा है, इस जीवन-गाथा को पढ़ कर पाठक गण अपने जीवन का रूपान्तरण करने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे तथा दिव्य जीवन के मार्ग के पथिक बनेंगे।
इस पुस्तक में वर्ष १९८१ तक की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
शिवानन्दनगर -द डिवाइन लाइफ सोसायटी
२९ जुलाई २००७
विषय-सूची
4. गुरुदेव के साथ युगान्तरकारी यात्रा
11. शिक्षा का भण्डार
12. दिव्य जीवन
प्रथम अध्याय
संस्कृति की गोद में
"शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ।
-योगभ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचरण वाले श्रीमान् पुरुषों के घर में जन्म लेता है" (गीता : ६-४१) ।
स्वामी चिदानन्द का जन्म तब मद्रास महाप्रान्त के अन्तर्गत मंगुलूरु में जागीरदारों के एक परम्परानिष्ठ महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। यह परिवार कुम्भकोणम् में आ बसा था। इसे शिवाजी के दिनों में जागीर प्राप्त हुई थी। इस परिवार को अँगरेजों के शासन काल में भी शासकीय संरक्षण निरन्तर प्राप्त होता रहा। इस कुल के ही श्री गोविन्द राव बीजापुरकर को ब्रिटिश राज्य की सेवाओं के लिए महारानी विक्टोरिया से कोयम्बतूर जिले में मैलेरपालयम् की जागीर प्राप्त हुई थी। इनके पौत्र सर्खिल गोविन्द राव तंजावूरु के राजप्रासाद में सम्पर्क-अधिकारी नियुक्त हुए थे तथा उन्हें वृत्तिभोगी महाराष्ट्रीय राजकुमारों की सम्पत्ति का कार्यभार दिया गया था। ज्ञानी बीजापुरकर के कुलक्रमागत इस समृद्ध तथा अभिजात परिवार ने अपनी कुलीनता तथा धर्मपरायणता के लिए ख्याति प्राप्त कर ली थी। गोविन्द राव बीजापुरकर के भतीजे ज्ञानी नारायण राव भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त आत्मा के रूप में ज्ञात थे।
सर्खिल गोविन्द राव एक उत्कृष्ट कोटि के दार्शनिक थे। वह असाधारण अन्तःप्रज्ञा से सम्पन्न थे। वह प्रायः लोगों के भविष्य के विषय में अक्षरशः सत्य भविष्यवाणी कर उन्हें आश्चर्यचकित कर देते थे। वह आत्मसन्तुष्ट थे तथा आभ्यन्तरिक चिन्तनमय कार्यनिवृत्तिपरक विविक्त जीवन-यापन करते थे। वह निर्धनों तथा दीनों पर बहुत अनुकम्पा प्रदर्शित करते थे। प्रतिदिन प्रथम कुछ भूखे लोगों को भोजन कराये बिना वह स्वयं भोजन नहीं करते थे। उनकी धर्मपत्नी कावेरी बाई भी अध्यात्म में विशेष उन्नत आत्मा थीं। वह तपस्विनी का-सा जीवन-यापन करती थीं। अपने पतिदेव गोविन्द राव के निधन पर उन्होंने शोक नहीं प्रकट किया अथवा व्यवहारानुरूप शोक मनाया। पतिदेव के मृत्यूपर। उनके जीवन में एकमात्र परिवर्तन जो देखने को मिला वह यह था कि वह श्वेत वस्त्र धारण करने तथा अतिसंयमी अन्तर्मुखी जीवन-यापन करने लगीं। शेष जीवनभर उन्होंने केवल दूध और फल पर निर्वाह किया। उनके प्रतिवेशी उनकी धर्मपरायणता तथा पवित्रता के लिए उनका बहुत सम्मान करते थे। वह समय-समय पर भक्तों को अपने घर पर आमन्त्रित करती और सत्संगों का संचालन करती थीं।
कावेरी बाई के पिता वेंकट राव राजमहल में सहचारी के रूप में कार्य करते थे। किन्तु वह केवल पदनाम में ही सहचारी थे। सांसारिक वस्तुओं के प्रति उनकी अनासक्ति लोक-प्रसिद्ध थी। तथ्य की बात तो यह है कि बहुत से लोग उन्हें सन्त मानते थे। वह कृष्ण के परम भक्त थे। मैसूर में राजप्रासाद के सामने अवस्थित अपने भवन में भगवान् श्रीकृष्ण की मूर्ति-जिसे आज तक 'कट्टे मने' नाम से पुकारा जाता है-प्रतिष्ठित की थी। एक जन्म-जात कवि की तरह भगवान् की स्तुति में भक्तिपूर्ण स्तोत्र उनसे स्वतः ही सहज भाव से निःसृत होते थे। उनके द्वारा रचित धरोहर में छोड़े गये-सैकड़ों स्तोत्र आज भी 'मध्व सम्प्रदाय' के अधिसंख्यक ब्राह्मण परिवारों द्वारा गाये जाते हैं। यद्यपि राज्य के पदानुक्रम में वह उच्च पद पर आसीन थे, पर उनका जीवन 'कमल-पत्र पर जल की बूंद' की परम्परागत भावना का एक आदर्श था। वह अपना घर भक्तों तथा सन्तों के लिए सदा खुला रखते थे। उनके पूजा महाकक्ष ने वास्तव में सार्वजनिक मन्दिर का रूप ले लिया था। इस पवित्र देवालय में लोग बहुत बड़ी संख्या में देवता के दर्शनार्थ आते रहते थे।[1]' वेंकट राव एक भगवत्साक्षात्कार प्राप्त आत्मा समझे जाते थे। वह कभी-कभी चेन्नै जाते और अपनी पुत्री कावेरी बाई के पास रहते। पिता-पुत्री का यह मिलन आध्यात्मिक सत्संग का वातावरण उत्पन्न किया करता था।
सर्खिल गोविन्द राव तथा सौभाग्यशालिनी कावेरी देवी के दो पुत्र-जी. कृष्ण राव तथा जी. श्रीनिवास राव-तथा एक पुत्री, गोपी बाई थी। जी. कृष्ण राव तथा जी. श्रीनिवास राव ने एक समृद्ध जमींदार के रूप में उन्नति की तथा तमिल नाडु के कोयम्बतूर जिले में अनेक ग्राम, मन्नार्गुडी जिले के तंजावूरु के पास विस्तृत भूमि तथा चेन्नै नगर में इधर-उधर बिखरे हुए अनेक भवनों को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। वे अपने पिता के साथ कोयम्बतूर में रहते थे जहाँ उनके पिता कार्यनिवृत्त जीवन-यापन करते थे। पिता के निधन के पश्चात् दोनों भाई कोयम्बतूर छोड़ कर चेन्नै नगर में बस गये।
कनिष्ठ भ्राता जी. श्रीनिवास राव 'किम्बली' नामक एक असम्बद्ध रूप से बनी पाचीन कोठी में निवास करते थे जो उस समय चेन्नै नगर के बाह्यांचल में पश्चिम की ओर अवस्थित थी। इनका विवाह सन् १९१० में मंगुलूरु के एक लब्धप्रतिष्ठ दम्पति नेलीकाई वेंकट राव तथा सुन्दरम्मा की पुत्री सरोजिनी देवी से हुआ। इस विवाह से दो बहुत ही समृद्ध तथा प्राचीन परिवारों का सम्मिलन हो गया। एन. वेंकट राव इतने अधिक लोकप्रिय थे कि वह मंगुलूरु नगरपालिका-समिति के निरन्तर तीन सत्रों में अध्यक्ष निर्वाचित होते रहे। उन्हें अपने पिता गुण्डू राव से, जो उत्कृष्ट कोटि के व्यापारी धे, काफी की विशाल भूसम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। वह 'मनोहर-विलास' नामक भव्य भवन में निवास करते थे। उनका मंगुलूरु के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव था। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुन्दरम्मा देवी एक बहुत ही धर्मनिष्व तथा सुसंस्कृत महिला थीं। उन्होंने 'देवरनामा' नामक प्रार्थनाओं की एक पुस्तक की रचना की जिसमें कन्नड़ भाषा के भक्तिपूर्ण गीतों का समावेश है। लोग उनका इतना अधिक सम्मान करते थे कि सन् १९४० में जब उन्होंने प्राण त्याग किया तो प्रायः सारा मंगुलूरु शोक प्रकट करने तथा उनके अन्तिम संस्कार में भाग लेने के लिए उमड़ पड़ा। उनके कोई पुत्र न था, केवल सरोजिनी, मनोरमा, मालती तथा मुक्ता नामक चार पुत्रियाँ थीं। सरोजिनी देवी उन सबमें ज्येष्ठ थीं। उनका पाणिग्रहण-संस्कार बारह वर्ष की आयु में चेन्नै के जी. श्रीनिवास राव के साथ हुआ। उन्होंने अपनी माँ से धार्मिक भक्ति-भावना उत्तराधिकार में प्राप्त की। उनमें प्राच्य परम्परा तथा पाश्चात्य जीवनचर्या का विलक्षण सम्मिश्रण था। उन दिनों 'मनोहर-विलास' में ठेठ पाश्चात्य रूप-रंग की झलक रहती थी। वहाँ उच्च सामाजिक पद के पुर्तगाली, डच तथा अन्य यूरोप जातीय लोग निरन्तर ठहरते थे। उनका जन्म तथा लालन-पालन पाश्चात्य-प्राधान्य वातावरण में हुआ। उनकी शिक्षा महिला-ग्ठ में हुई। उनकी उपलब्धियों में कुशल पियानोवादन के साथ सुन्दर अँगरेजी में भजन गा सकने की क्षमता की गणना की जाती थी। वह टेनिस खेलने में प्रवीण थीं।
सरोजिनी देवी की पहली सन्तान पुत्री हुई जिसका नाम माता-पिता ने हेमलता रखा। हेमलता के जन्म के दो वर्ष पश्चात् सरोजिनी देवी ने भाद्रपद के कृष्णपक्ष की द्वादशी तिथि तदनुसार रविवार २४ सितम्बर १९१६ पूर्वाह्न के १०.३५ बजे 'मनोहर-विलास' में एक सिद्ध, भावी स्वामी चिदानन्द को जन्म दिया। वैष्णव माता-पिता ने बच्चे का नाम श्रीधर रखा। बच्चे की स्नेहमयी फूफी गोपीबाई उन्हें 'सिद्ध' कह कर पुकारा करती थीं जो कि श्रीधर का श्रुतिमधुर संक्षिप्त रूप है। बालक की जन्मपत्री तैयार करने वाले ज्योतिषी ने लिखा कि बालक इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त करेगा। इसकी पुष्टि एक प्रख्यात योगी ज्योतिषी ने सन् १९४९ में यह घोषणा कर की : "चिदानन्द जी अपने गत जन्म में ही एक महान् योगी तथा सन्त थे। यह उनका अन्तिम जन्म है।" बालक का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ। राहु तीसरे, गुरु छठे; शुक्र, शनि तथा केतु नवें, चन्द्रमा दशवें, बुध तथा सूर्य ग्यारहवें तथा मंगल बारहवें गृह में थे। केतु की नवें गृह में स्थिति मोक्ष की सम्भावना रखती है। शनि तथा शुक्र का नवें गृह में होना राजयोग तथा भक्तियोग के प्रति गहरी अभिरुचि का द्योतक है। सरोजिनी देवी ने बालक की जन्मपत्री एक प्रवीण ज्योतिषी की सहायता से तैयार करायी और उसे अपने हाथों से देवनागरी लिपि में लिख कर सुरक्षित रख लिया। श्रीधर की जन्मपत्री की सारणी निम्न प्रकार है :
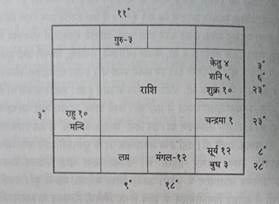
जन्म के पाँच वर्ष, सात माह और आठ दिन तक केतु की महादशा थी। श्रीधर का जन्म-नक्षत्र मघा का प्रथम चरण था तथा उनकी जन्म-राशि सिंह थी। जन्मपत्री यह सूचित करती थी कि आने वाले दिनों में उन्हें भव्य, असाधारण व्यक्तित्व प्राप्त होगा।
श्रीधर के जन्म के दो वर्ष पश्चात्, जब सरोजिनी देवी पुनः गर्भवती थीं, श्रीनिवास राव में अकस्मात् तीव्र वैराग्य-भाव विकसित हुआ और एक दिन वह चुपके से घर से लुप्त हो गये। वह रायचूर के समीप मन्त्रालय में स्थित श्री राघवेन्द्र स्वामी के पवित्र समाधि-मन्दिर में पलायन कर गये जहाँ वह चिरकाल तक अज्ञात रूप से रुके रहे। श्री राघवेन्द्र स्वामी ने अपना नश्वर शरीर पाँच सौ वर्ष पूर्व त्यागा था; किन्तु शरीर के बन्धनों से मुक्त रहने की दशा में भी वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देते तथा उनका पथप्रदर्शन करते रहते हैं। एक दिन श्रीधर के ताऊ कृष्ण राव ने अन्तर्वाणी सुनी : "मैं मन्त्रालय का स्वामी राघवेन्द्र तुमसे बोल रहा हूँ। श्रीनिवास राव मेरे पास हैं। चिन्ता न करें। वह शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट जायेंगे।" सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कृष्ण राव की इस आश्चर्यजनक अनुभूति के तुरन्त बाद ही श्रीनिवास राव वास्तव में किम्बर्ली वापस आ गये। इस बार सरोजिनी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महान् राघवेन्द्र स्वामी की कृपा की स्मृति में बालक का नाम राघवेन्द्र रखा गया। तदनन्तर सरोजिनी देवी की दो और कन्याएँ हुईं जिनका वसुधा तथा वत्सला नामकरण किया गया। ये सभी बच्चे अपना अधिक समय मंगुलूरु में अपने नाना के निवास-स्थान 'मनोहर-विलास' में व्यतीत करते थे।
सरोजिनी देवी एक आदर्श गृहस्वामिनी थीं। उनकी विमल शुचिता तथा भक्ति ने श्रीधर के हृदय पर अपनी छाप अंकित की। वह प्राचीन काल की रानी मदालसा की भाँति ही अपने इस यशस्वी शिशु को प्रथम पाठ की शिक्षा देने वाली माँ थीं। वह मीराबाई, रैदास, कबीरदास तथा नरसी मेहता के भजन गाया करतीं और हिमालय के सन्तों की गाथाएँ सुना कर अल्पवयस् बालक को आनन्दित किया करती थीं। प्रतिदिन सोने के समय श्रीधर अपनी माँ से लिपट जाते तथा भजन अथवा कहानी की माँग करते। स्नेहमयी माँ कभी भी उन्हें निराश नहीं करती थीं। वह अपने श्रुतिमधुर स्वर में भक्तिमय गीत गुनगुनार्ती और ऋषियों-मुनियों के आख्यान वर्णन करतीं। इन भजनों तथा आख्यानों से श्रीधर एक प्रकार से अनुप्राणित से हो जाते। इस भाँति उनकी माता जी ने उनके व्यक्तित्व के घटन में जो गहरी छाप डाली उसे वह परवर्ती काल में व्याख्यान देते समय कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते करते हैं।[2] इसे संघिनी वन्दना ने अपने लेख 'गुरु, आश्रम तथा ईसाईजन' में अंकित किया है। इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि स्वामी जी जब पूना के 'क्राइस्ट प्रेम सेवाश्रम' में पधारे तो उन्होंने मीराबाई के उस गीत को किस प्रकार स्मरण किया जिसे उनकी माता ने उन्हें सुलाने के लिए एक बार गाया था। इस भजन में भावविभोर हो नृत्य करते समय मीरा का भगवान् में विलय का वर्णन

माता श्री सरोजनी देवी
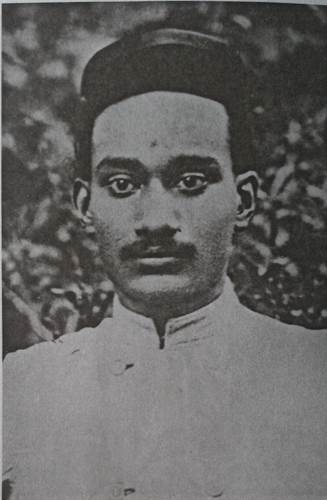
पिता श्री श्रीनिवास राव

माता श्री की गोद में

मनोहर विलास में
बायें से दाहिने खड़े हुए-मौसी मालती, श्रीधर (स्वामी जी), नाना श्री वेंकट राव, बड़ी बहन हेमलता और उसके आगे मौसी मुक्ता बायें से दायें बैठे हुए-छोटे भाई श्री राघवेन्द्र, नानी श्रीमती सुन्दरम्मा देवी, बहन वत्सला, मौसी मनोरमा और उसके आगे बहन वसुधा बायें से दाहिने खड़े हुए-मौसी मालती, श्रीधर (स्वामी जी), नाना श्री वेंकट राव, बड़ी बहन हेमलता और उसके आगे मौसी मुक्ता बायें से दायें बैठे हुए-छोटे भाई श्री राघवेन्द्र, नानी श्रीमती सुन्दरम्मा देवी, बहन वत्सला, मौसी मनोरमा और उसके आगे बहन वसुधा
है जब मीरा अदृश्य हो गयीं और उनकी साड़ी देव-विग्रह के साथ लटकी हुई मिली। स्वामी जी ने बतलाया कि वह किस प्रकार इस भगवान् में विलय की कहानी से प्रभावित हुए थे। ऐसी थी वह शिक्षा जिसे माँ सरोजिनी ने अपने प्रिय पुत्र को प्रदान किया और जिसे इन्होंने कभी विस्मृत नहीं किया। निस्सन्देह यह ठीक ही कहा गया है कि 'पालना झुलाने वाला हाथ संसार पर शासन करता है।'
बाल्यकाल में श्रीधर के कनिष्ठ भ्राता राघवेन्द्र उनके क्रीड़ा-साथी तथा उनके मातामह के वृद्ध सहचर अनन्तैया उनके सतत साथी थे। अनन्तैया एन. वेंकट राव के परिवार के साथ बहुत दिनों तक रहे थे। उनके साथ प्रायः परिवार के एक सदस्य के रूप में व्यवहार किया जाता था। वह श्रीधर, राघवेन्द्र तथा परिवार के अन्य बालकों की खेल के समय देख-रेख किया करते थे। बालक अरब सागर से मिलने के अन्तिम चरण में आनन्दपूर्वक प्रवहमान उद्विग्न नेत्रवती सरिता के तट पर प्रायः खेला करते थे। अरब सागर के क्षितिज पर सूर्यास्त दिनभर की क्रीड़ा की समाप्ति का संकेत था; किन्तु बालक फिर भी रुके रहते। श्रान्त तथा क्लान्त वे अपने हाथ-पैर बालुका में गाड़ देते और कहानी के लिए अनन्तैया को परेशान करते। इस वृद्ध परिचर ने जैमिनि भारत, रामायण तथा भागवत महापुराण से कहानियों का अक्षय भण्डार संग्रह कर रखा था। वह उन्हें एक कहानी सुना कर आह्लादित करने को सदा उद्यत रहते। ऐसे अवसरों पर श्रीधर उन वृद्ध सज्जन के ओष्ठों से निःसृत भक्ति-धारा को छक कर पान करते हुए मौन तथा मुग्ध हो बैठे रहते। कहानी समाप्त होने तक अन्धकार सघन हो उठता। अब वृद्ध सज्जन रुक जाते और बालकों से प्रश्न करते: “तुम किसके समान बनोगे?" द्युतिमान् तथा गम्भीर दृष्टि से आलोकित मुखमण्डलयुक्त श्रीधर निरपवाद रूप से यह उत्तर देते: "मैं ऋषि बनूँगा।" इस पर वृद्ध सज्जन खिलखिला कर हँस पड़ते और मुख बना कर कहते : "तू नुशी बनेगा।" कन्नड़ भाषा में 'नुशी' का अर्थ मच्छर है। भला वृद्ध सज्जन अनुमान भी कैसे कर सकते थे कि श्रीधर वास्तव में एक सिद्ध हैं और असंख्य जिज्ञासुओं का पथ-प्रदर्शन करने के लिए जन्म ग्रहण किये हैं। जहाँ तक श्रीधर का सम्बन्ध है उनका अभिप्राय उनके कथन के अनुरूप ही था। कभी-कभी वह अपनी मौसी मालती बाई से अपनी गोपनीय बात कहते थे कि वह प्राचीन कालीन ऋषियों की भाँति अरण्य तथा निर्जन कन्दराओं में जा कर एकान्त में ध्यान करना चाहते हैं। ऋषि बनने का विचार इतना प्रबल था कि एक दिन वह वास्तव में कौपीन धारण कर तथा भस्म की भाँति सारे शरीर पर टैल्कम पाउडर लगा कर व्याघ्र-चर्म पर पालथी मार कर बैठ गये और प्रार्थनाशील भाव से अपने नेत्र बन्द कर भगवान् के आगमन की गम्भीरता से प्रतीक्षा करने लगे।
इस प्रकार बाल्यकाल व्यतीत होता गया। एक बार दादी कावेरी बाई बहुत से नौकर-चाकरों के साथ उत्तरी भारत के तीर्थस्थलों की यात्रा पर गयीं। अपनी तीर्थयात्रा से वापस आने पर उन्होंने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के सम्मुख अपनी तीर्थयात्रा के पावनकारी अनुभव को बड़ी ही भाव-प्रवणता से वर्णन
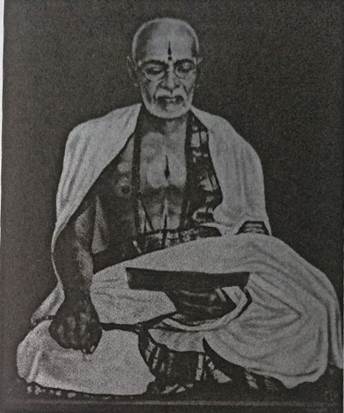
सहचारी श्री वेंकट राव

मनोहर विलास
किया। श्रीधर के लिए दादी का वृत्तान्त एक यात्री जीव का रोमांचकारी विवरण था। स्वामी जी ने एक निजी भेंटवार्ता में उल्लेख किया कि वह उनके जीवन का सर्वप्रथम अवसर था जब गंगा तथा हरिद्वार की महिमा का निस्वन उनके कर्णकुहरों तक पहुँचा।
श्रीधर तथा राघवेन्द्र कभी-कभी अपने पिता के पास चेन्नै की किम्बर्ली कोठी में रहा करते थे, जब उनके प्रमातामह 'सहचारी' वेंकट राव अपनी पुत्री कावेरी के साथ कुछ दिन रहने के लिए वहाँ आया करते थे। एक बार इस प्रकार के आगमन के समय कावेरी बाई ने श्रीधर को उन्हें नमस्कार करने के लिए कहा तथा उनके कान में सत्य भाव से यह फुसफुसाया कि उनके पिता (वेंकट राव) कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वरन् एक महान् भक्त हैं जिन्हें श्रीकृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त है ।[3] इन शब्दों को सुन कर श्रीधर पुलकित हो उठे तथा उन्होंने अपने प्रमातामह के रूप में ऐसे भागवत पुरुष के पावनकारी दर्शन कर उद्दीप्त अनुभव किया। उन्होंने मन-ही-मन यह संकल्प किया कि एक दिन वह भी अपने प्रमातामह के समान महान् भक्त बनेंगे और भगवद्दर्शन करेंगे।
श्रीधर के पावन यज्ञोपवीत-संस्कार का शुभ अवसर यथा-समय आ पहुँचा। परिवार के लोगों ने मांगलिक उपनयन-संस्कार अपने कुलदेवता भगवान् वेंकटेश्वर के पवित्र धाम तिरुपति में सम्पन्न करने का निश्चय किया। धर्मक्रिया समाप्त होने पर जब सब लौट रहे थे, एक दुकान में श्रीराम की मनोरम मूर्ति पर श्रीधर आकर्षित हुए और अपने माता-पिता से उसे क्रय करने के लिए अनुनय किया। यह निवेदन सुन कर माता-पिता प्रसन्न हुए और उनके लिए वह श्री कोदण्ड राम की प्रतिमा खरीद दी।
उसके पश्चात् श्री कोदण्ड राम को 'मनोहर-विलास' के बालकों के जीवन में प्रमुख स्थान ग्रहण करना था। प्रतिमा को कुल-देवता के पार्श्व में स्थापित कर दिया गया और सभी महत्त्वपूर्ण अवसरों पर उसकी वैधिक पूजा की जाती। श्रीधर अब आध्यात्मिक अनुशासन के पालन तथा विध्यात्मक पूजा में अत्यधिक सतर्क पाये जाते। दैनिक सन्ध्या-वन्दन करने से पूर्व वह कभी भी भोजन नहीं ग्रहण करते थे जैसा कि पवित्र यज्ञोपवीत-संस्कार के पश्चात् ब्राह्मणों के लिए विधान है। वह प्रतिदिन अपनी मौसियों, भाई तथा बहनों के साथ श्री कोदण्ड राम के चरणों में बैठ जाते और प्रार्थनाशील पूजा निवेदन करते। यह उन सबके लिए एक मनोहर क्षण हुआ करता। श्रीधर के पूजा करते समय एक चमत्कारिक वस्तु देखने में आती। जब वह भगवान् को पुष्प अर्पित करते, उनके मस्तक पर सुगन्धित चन्दन तथा कुंकुम लगाते, नीराजन करते, तब प्रतिमा असाधारण प्रोज्ज्वल प्रभामण्डल से चमक-सी उठती तथा भगवन्मुखमण्डल पर स्वर्गिक मुस्कान छा जाती। किशोर भक्त इसे प्रायः प्रतिदिन ही देख सकते थे और वे इस भगवत्कृपा के प्रकटीकरण से आनन्द से पुलकित हो उठते। ऐसे भी दिन होते जब मूर्ति के चतुर्दिक् प्रभा न भी दमकती। ऐसे समय उनके विषाद की सीमा न रहती। वे उस स्वर्गिक प्रकाश की झलक पाने के लिए प्रतीक्षा करते और आँख चुरा कर मूर्ति की ओर देखते। तब श्रीधर आगे आते और सबसे कहते, "आप लोगों ने कोई अयोग्य कार्य अवश्य किया है अथवा किसी महत्त्वपूर्ण विषय की उपेक्षा की है जिससे भगवान् अप्रसन्न हैं। आइए, हम सब गम्भीर उत्साह तथा प्रेम के साथ दण्डवत् प्रणाम तथा प्रार्थना करें।" ऐसा कह कर वह भगवान् के सम्मुख करबद्ध हो अनुनय-विनय करते और भगवान् से प्रार्थना करते कि वह दया करके उनकी भूलों को क्षमा कर दें और अपने द्युतिमान् रूप में एक बार पुनः प्रकट हों। और देखें ! वह मूर्ति पुनः उसी पुरानी द्युति तथा कृपा से दमक उठती।'[4]
श्रीधर ने एक पुरानी धर्म घड़ी के आधार से भगवान् कोदण्ड राम के लिए एक रथ तैयार किया। वह श्री राम की मूर्ति को इस रथ पर आम्रवाटिका में ले जाया करते थे। इस प्रकार की रथ-यात्रा के उत्सवों के अवसर पर यह किशोर भक्त भाव-विभोर हो उठता और कभी-कभी वह चिन्तनशील अवस्था में बैठ जाता और निश्चयपूर्वक घोषणा करता : "मैं योगी बनूँगा।" घर में एक वृद्ध नौकर था जिसका नाम बालू था। उसे यह निश्चय हो गया था कि श्रीधर योग-शक्ति से सम्पन्न हैं। वह श्रीधर के हाथों से पवित्र चरणामृत लेने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करता था। उसकी यह दृढ़ धारणा थी कि श्रीधर द्वारा वितरित पवित्र चरणामृत ने उसका चिरकालिक उदर-रोग ठीक किया था। इस भाँति किशोर श्रीधर के सन्तत्व के विषय में परिवार के लोगों के अपने-अपने अनुभव थे।
श्रीधर अपनी आभ्यन्तर सत्ता में भावी सिद्ध का आकार ले चुके थे; किन्तु अपने दैनन्दिन जीवन में वह एक सामान्य स्वस्थ बालक की तरह व्यवहार करते थे। निर्दोष क्रियात्मक परिहास करना उन्हें प्रिय था। पहाड़ियों तथा मीनारों पर आरोहण करने में वह आनन्दित होते थे। वह निर्भीक तैराक भी थे। उन्होंने एक बार अपनी मौसी मालती बाई को डूबने से बचाया। वह सभी प्राणियों से प्रेम करते और उनके साथ दयालुता से व्यवहार करते थे। दश वर्ष की अल्पायु में भी वह असाधारण विनम्र भाव अभिव्यक्त करते थे। एक बार इनके मातामह तथा मातामही दीर्घावकाश के लिए समस्त
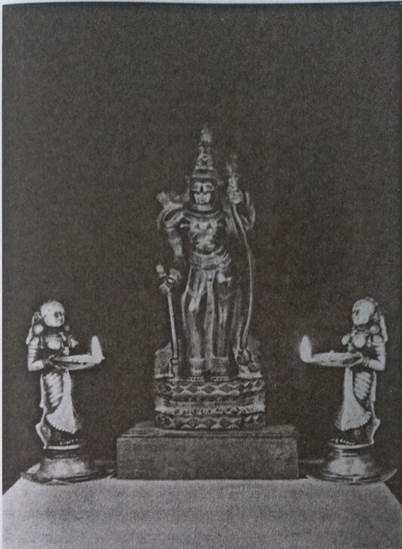
श्री कोदण्ड रामस्वामी जी द्वारा बचपन में स्थापित

श्री गोपाल कृष्ण (श्री वेंकट राव द्वारा प्रतिष्ठित)
परिवार को बेंगुलूरु ले गये। एक दिन सायंकाल जब परिवार के सभी गुरुजन सैर के लिए गये हुए थे, श्रीधर ने सभी बच्चों से विचार-विमर्श किया कि वे किस प्रकार प्रतिदिन जानबूझ कर अथवा अनजान में भूलें करते रहते हैं और उनसे यह स्वीकार कराया कि उन्हें गुरुजनों से क्षमा-याचना करनी चाहिए। इस प्रकार इनसे उत्प्रेरित हो कर उन सबने स्नान किया और गुरुजनों के वापस आने पर भीगे वस्त्र धारण किये हुए ही उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया। यद्यपि गुरुजनों ने इस प्रदर्शन को यथावत् पसन्द नहीं किया और उन्हें किंचित् फटकारा भी; किन्तु यह घटना श्रीधर अपने विचार तथा वाणी में उस समय जो धर्म-परायणता प्रतिबिम्बित करते थे, उसको प्रकट करती है।
बालक के रूप में श्रीधर को जीवन से स्नेह था। वह विनोद तथा निर्दोष नटखटपन से पूर्ण थे। उन्हें अपनी नकल करने की क्षमता का प्रदर्शन करना प्रिय था। निस्सन्देह वह एक अच्छे अभिनेता थे। मंगुलूरु के उनके आवास-काल में एक ईसाई विधिवक्ता, जो अव्यवसायी नाट्यकला के अभिनयों के प्रदर्शन का आयोजन किया करते थे सदा ही बालक श्रीधर से अपने नाटकों में भाग लेने के लिए आग्रह किया करते थे। इस भाँति अपनी वय के सामान्य बालक की तरह उन्हें जीवन, प्रकृति तथा कला से स्नेह था। इसके साथ ही उनमें ऊधमीपन से मेल खाने वाला गाम्भीर्य, धर्म तथा अधर्म के प्रति असाधारण संवेदनशीलता तथा तीव्र धार्मिक उत्साह था जो उन्हें सामान्य बालकों से अलग करता था। मान नही सुन्दरम्मा ने अपने दौहित्रों तथा दौहित्रियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने के लिए सभी सम्भव उपाय किये। वह उन्हें मंगला देवी के मन्दिर में ले जाया करती थीं। ' नोहर-विलास' में एक विशाल महाकक्ष था जहाँ वह हरिकथा तथा सत्संगों का आयोजन किया करतीं। वह श्रीमद्भागवत सप्ताह के लिए विख्यात पण्डितों को आमन्त्रित किय, करती थीं। श्रीधर इन सब प्रवृत्तियों में अपनी गहन रुचि के कारण विशेष प्रख्यात थे इस प्रकार के हरिकथा-सत्र-काल में एक दिन उन्होंने एक पण्डित से दो अर्थगर्भित तथा सुप्रसिद्ध कहानियाँ सुनीं। उनमें से एक में उस मेढक की चेष्टा का वर्णन है जो मृत्यु वः मुख में जा पड़ा था। उसे जब एक साँप निगल रहा था, उसके ऊपर से एक व्याध-पतंग उड़ा और मेढक ने उस नाजुक स्थिति में होते हुए भी उस बेचारे कीट को पकड़ने के लिए अपने शरीर को एक झटका दिया। यह कहानी संसार में बद्ध जीवों के स्वरूप को स्पष्ट करती है। दूसरी कहानी वर्णन करती है कि एक चाँदनी रात में जंगल में विचरण करता हुआ एक व्यक्ति किस प्रकार कुएँ में गिर पड़ा। जब वह गिरते हुए नीचे आधी दूर था, तब एक पौधे को पकड़ने में सफल हो गया जो कुएँ की दीवाल के एक रन्ध्र में उग आया था। इस पौधे के चारों ओर एक सर्प कुण्डली मार कर बैठा था और धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा था। अत्यधिक आतंक से जब ऊपर की ओर दृष्टि की तो उसने ऊपर भूमि-तल पर नीचे अपनी ओर देखते हुए व्याघ्र के मुख को देखा। उसने अपने से नीचे की ओर एक मकर को अपने जबड़े खोले हुए इसकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। इसी समब ऊपर के एक वृक्ष में लगे हुए मुधकोश से मधु की कुछ बूँदें टपकीं। लटकते हुए व्यक्ति ने अपना मुख विवृत किया तथा मधु की कुछ बूँदें पकड़ने के लिए अपनी जिह्वा बाहर निकाली। यह संसार की विभीषिका तथा जीव की मोहावस्था का एक अन्य रूपान्तर है। इन दोनों शिक्षाप्रद कहानियों ने श्रीधर के मन पर अपनी चिरस्थायी छाप डाली।
श्रीधर के 'मनोहर-विलास' के आवास के दिन इन विविध प्रकार की अनुभूतियों, कार्यों तथा विचारों से सम्भृत थे। यह निश्चय ही संस्कृति की वह गोद थी जहाँ उनमें सत्तारूढ़ आन्तरिक व्यक्तित्व का पोषण हुआ तथा आने वाले दिनों में दैवनिर्दिष्ट रेखा के साथ-साथ बढ़ने के लिए उसे तैयार किया गया। उत्कृष्ट विचार उनकी चेतना को सदा आच्छादित किये रहते। श्रीधर में सत्तारूढ़ सन्तत्व ने परिवार द्वारा प्रदत्त उन सब भावोत्तेजक संस्कारों को अपनी सत्ता के अन्तरतम प्रदेश में सँजोये रखा। इस भाँति प्रारम्भ से ही पासा फेंक दिया गया। यद्यपि उनका भव्य भविष्य, उस समय लोक-दृष्टि से अधिकांश ओझल था; किन्तु उनके हृदय के निगूढ़ प्रदेश में उसका प्रारम्भिक प्रकटन होने लग गया था। बीज का वपन किया जा चुका था। उसके अंकुरित, ऊँचा तथा बलवान् होने तथा सभी दिशाओं में राजपथ पर अगण्य श्रान्त पिपासु आत्माओं को फल तथा छाया प्रदान करने वाली अपनी प्रसरणशील शाखाओं को विस्तारित करने में समय की आवश्यकता थी।
द्वितीय अध्याय
ईश्वर की खोज में
"यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।
- जिस नाशवान् क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूतप्राणी जागते हैं
वह तत्त्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि हैं" (गीता : २-६९) ।
श्रीधर सात वर्ष की आयु में सेण्ट ऐन के विहार में प्रविष्ट हुए। माँ सरोजिनी देवी ने, जिन्हें इसी विहार में शिक्षा प्राप्त हुई थी, इनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। वह इस ओर विशेष रूप से सावधान थीं कि उनका अँगरेजी भाषा का आधार दृढ़ हो। यहाँ इस बात पर ध्यान देना रोचक होगा कि इस भावी स्वामी के शैक्षिक जीवन के प्रारम्भ से अन्त तक की पढ़ाई-लिखाई ईसाई शिक्षा से अनुप्राणित प्रधानतः पाश्चात्य रंग में रंगे शैक्षिक परिसर में हुई। अँगरेजी की शिक्षा न केवल इनके स्वभाव में आधुनिकता लायी वरन् इनको उदार दृष्टिकोण से भी सम्पन्न बना दिया।
एक वर्ष तक सेण्ट ऐन में रहने के पश्चात् वह रोज़रियो माध्यमिक विद्यालय में प्रविष्ट हुए जहाँ उन्होंने तृतीय श्रेणी (आठवीं कक्षा) तक अध्ययन किया। उनके छात्र-जीवन की प्रारम्भिक अवस्था से ही उनके सहपाठी उनके कुछ आध्यात्मिक गुणों से प्रभावित थे। रोज़रियो स्कूल में इनके सहपाठियों में से देवीदास गिरधरलाल चन्द्राना थे जो आजकल मंगुलूरु के एक प्रख्यात धनीमानी व्यवसायी हैं। वह श्रीधर के विषय में इस प्रकार स्मरण करते हैं: "इस महान् आत्मा के सम्बन्ध में मेरी स्मृति यह है कि वह अपने अध्ययन में सामान्य वर्ग से बहुत ही ऊँचे, प्रतिभाशाली तथा मेघावी थे। उनका मुखमण्डल सदा ही कान्तिमय तथा द्युतिमान रहता था। इसके साथ ही हम उनके जीवन के उषाकाल के उन दिनों में भी उन्हें सदा धर्म तथा दर्शन के ग्रन्थों में रुचि लेते हुए पाते थे। वह कभी भी कोई समय व्यर्थ नष्ट नहीं करते थे। वह एक अतोषणीय पाठक थे। निस्सन्देह, उनकी बैडमिण्टन जैसे खेलों में रुचि थी। वह पैदल सैर करना पसन्द करते थे तथा प्रकृति और उसके सुरम्य सौन्दर्य में आनन्द प्राप्त करते थे। यद्यपि वह सदा प्रफुल्ल रहते थे तथापि ऐसा प्रतीत होता कि उनका मन कहीं अन्यत्र लगा हुआ है। उनके इने-गिने मित्र थे जिन्हें वह अब भी स्मरण करते हैं और उन्हें स्मरण करने तथा उनसे मिलने को महत्त्व देते हैं। दैववश उनका घर तथा मेरा घर एक राजपथ पर थे तथा परस्पर बहुत ही सन्निकट थे। हम प्रतिदिन घर से विद्यालय एक साथ ही आया-जाया करते थे। इससे मुझे उनके निकट सम्पर्क में आने का लाभ हुआ। कभी-कभी मुझे यों ही ऐसा दिखता कि वह एक दिन स्वामी बनेंगे। मुझे यह पता नहीं कि ऐसा सोचने को मुझे किसने प्रेरित किया; किन्तु यह विचार स्वतः प्रवर्तित था। कदाचित् इनके अभिजात परिवार के होने के बावजूद भी उन्हें सादा जीवन-यापन करते देख कर ऐसा लगा हो। उनकी आवश्यकताएँ न्यूनतम थीं तथा उन्हें सादा जीवन पसन्द था। सम्भवतः इन सभी कारणों से प्रभावित हो कर ही मैंने ऐसा कहा था कि वह एक दिन एक महान् स्वामी बनेंगे। किसी ने उनके साथ चाहे कैसा भी अन्याय किया हो; किन्तु वह किसी के प्रति भी किसी समय कर्णकटु शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। जब कभी भी इस विषय पर चर्चा चलती तो वह सदा ही अपने मित्रों को सन्मार्ग पर आगे बढ़ने तथा विपथगामी न बनने के लिए प्रेरित किया करते थे।"
यद्यपि श्रीधर का पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा पाश्चात्य प्रणाली से हुई; किन्तु वह प्राची की ही सन्तान बने रहे। इन्हें जो शिक्षा प्राप्त हुई वह इन्हें पाश्चात्य रंग में न रँग सकी; क्योंकि जिस पारिवारिक वातावरण में वह रह रहे थे वह हिन्दू-जगत् के प्राचीन नैतिक मूल्यों के सलिल से स्नात था। इस भाँति प्राचीन प्राच्य जगत् तथा आधुनिक पाश्चात्य जगत् के मध्य संयोजक का काम करना उनकी नियति थी। बालक-रूप में उन्होंने सन्त-महात्माओं की जो गाथाएँ सुनी थीं, वे उनके चित्त में गहराई तक प्रवेश कर गयी थीं। उन्होंने ही इनकी आकांक्षाओं को आकार प्रदान किया। परम सत्ता की मूर्ति के रूप में पूजा को न केवल उनकी नित्य चर्या में अपितु उनकी सत्ता के आभ्यन्तर प्रदेश में स्नेह का चिरस्थायी स्थान प्राप्त था। भगवान् राम उनके हृदय के सिंहासन पर पहले से ही प्रतिष्ठापित हो चुके थे। कोदण्ड राम की पवित्र मूर्ति, जिसे वह अपने उपनयन-संस्कार के स्मृति-चिह्न के रूप में तिरुपति से लाये थे, 'मनोहर-विलास' के पुण्य निवास-स्थान के उनके जीवन में केन्द्र-बिन्दु का स्थान ले चुकी थी।
इसी अवधि में एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसका श्रीधर के आध्यात्मिक जीवन पर प्रबल प्रभाव पड़ना था। उन्हें एक ईश-मानव के, एक ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आने का संयोग हुआ जिसका राम-नाम प्राण ही था तथा जो भारत के जन-जीवन पर अत्यधिक प्रभाव रखता था। जब महात्मा गान्धी मंगुलूरु में एक प्रार्थना-सभा को सम्बोधित कर रहे थे तब अष्टवर्षीय बालक श्रीधर को अपने मातामह एन. वेंकट राव, जो समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे, के साथ उनके पास बैठने का पुण्य सद्भाग्य प्राप्त हुआ। बालक होते हुए भी वह इस सत्य तथा अहिंसा के ईश्वर-दूत के आध्यात्मिक चुम्बकत्व से सम्मोहित हो गये। यह इनके जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण बना रहा। बापू जी ही परिवार से बाहर के प्रथम आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिसने श्रीधर पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला, ऐसी अन्त:प्रेरणा दी जो इस भावी स्वामी के लिए आजीवन सँजोये रखने की विधि बन गयी। चौबीस वर्ष के अनन्तर श्रीधर उनसे पुनः मिले। इस बार वह स्वामी शिवानन्द जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में भंगी बस्ती, दिल्ली गये। उस समय महात्मा जी ने 'भाग्यशाली पुरुष' कह कर उनका स्वागत किया। आज भी वह गान्धी जी के साथ प्रथम मिलन को अपने जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना अनुभव करते हैं। उन्होंने कोदण्ड राम की मूर्ति में भगवान् के दर्शन किये थे। अब उन्होंने एक ईश-मानव के दर्शन किये जिसका प्राण राम-नाम के साथ स्पन्दित होता था।
उनके जीवन का आगामी प्रमुख अनुभव था परम प्रिय माता का निधन। उनकी मृत्यु असामान्य परिस्थिति में हुई। चेन्नै में 'किम्बर्ली' के अपने आवास-काल में वह एक दिन अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाड़ी से समुद्र तट पर गयीं जहाँ सैर करते समय पत्थर के एक टुकड़े से उन्हें ठोकर लग गयी। उनके बायें पैर में कुछ पीड़ा होने लगी और थोड़ी सूजन आ गयी। इसने कुछ ही घण्टों में ऐसा गम्भीर रूप ले लिया कि चिकित्सक को पाँव का अंगच्छेद करने का निर्देश देना पड़ा। किन्तु मृत्यु ने इसके लिए भी समय नहीं दिया और ३ जून १९२६ को अट्ठाईस वर्ष की आयु में सरोजिनी देवी की संसार-यात्रा समाप्त हो गयी। परम प्रिय माँ की मृत्यु किशोर श्रीधर के लिए संघातक अनुभव था। इस भूलोक में उनके लिए अपनी परम प्रिय माता से अधिक कुछ भी प्रिय न था जो माँ होने के साथ-ही-साथ उनकी आदि गुरु भी थीं। वह दशवर्षीय सुकुमार ही थे जब मृत्युदेव ने उनसे उनकी अतीव प्रिय वस्तु को छीन लिया। भीषण शक्ति से मृत्यु का अटल तथा अननुमेय स्वरूप उनकी समझ में आया। उन्हें संसार के दुःख का स्मरण हुआ। उन्हें भगवान् कोदण्ड राम की स्मृति आयी। उन्हें महात्मा गान्धी की प्रार्थना-सभा की याद आयी और जिस समय वह अपनी माँ की क्षति के लिए शोक कर रहे थे, उसी समय यह सत्य उन्हें स्पष्ट हो गया कि सांसारिक जीवन मिथ्या है तथा सन्तजन मर्त्य मानव के लिए उपलब्ध एकमात्र सन्मार्ग प्रदर्शित करते हैं।
सरोजिनी देवी की मृत्यु से श्रीनिवास राव सांसारिक कर्तव्यों तथा आनन्दों से सर्वथा उदासीन हो गये। वह अपने बच्चों को 'मनोहर-विलास' के परम विशिष्ट वर्ग के वातावरण से चेन्नै में 'किम्बर्ली' के कठोर एकाकीपन के वातावरण में वापस ले आये। इससे श्रीधर की विहार-शिक्षा में अल्पकालिक अन्तराल आया। पिता श्रीनिवास राव ने दोनों पुत्रों को सी. आर. सी. नामक पाठशाला में, जो पुरुषवाकम् महल्ला में स्थित थी, में प्रवेश (दाखिल) करा दिया। वी. सुब्बैया प्राइवेट ट्यूटर प्रतिदिन श्रीधर राव और उनके अनुज एस. राघवेन्द्र राव-जिसे लाड़ से रघु पुकारा जाता था-तथा दो और अग्रजों फुफेरा भाई बाबू और चचेरा भाई छोटू को भी घर पर आ कर पढ़ाता था ताकि मद्रास स्कूल-जिसमें शिक्षा माध्यम तमिल भाषा थी-में उन्हें प्रवेश दिलाया जा सके। किन्तु उनका पाठशाला जाना अल्पकालिक ही रहा था। कारण कि एक दिन पिता श्रीनिवास राव बच्चों की पाठशाला पुरुषवाकम् गये तो वहाँ के अस्वच्छ-मलिन-गन्दे वातावरण से उन्हें ऐसी वीभत्सा (उत्पन्न) हुई कि उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षण के लिए वहाँ उस शाला में न भेजने का तत्काल निर्णय ले लिया। यह क्रोधावेश से उत्पन्न असामान्य निर्णय था। क्रोध शीघ्र ही शान्त हो गया और वह लौकिक कर्तव्य के प्रति उदासीनता की सामान्य मनोदशा में पुनः जा पड़े। बच्चों की शिक्षा की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, इससे श्रीधर राव कुछ समय तक विध्यनुरूप शिक्षा के बिना ही रहे।
उस समय श्रीनिवास राव एक असाधारण स्थिति से, अपनी वैयक्तिक सुख-सुविधाओं तथा ऐहिक दायित्वों के प्रति भावशून्य अवस्था से गुजर रहे थे। वह पूजा में घण्टों निमग्न रहा करते। वह वंश परम्परा प्राप्त गुण तथा स्वभाव से अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति थे। वर्षों पूर्व वह एकान्तवास तथा शान्ति के लिए मन्त्रालय को पलायन कर गये थे, जो एक परम वन्दनीय सिद्ध महात्मा श्री राघवेन्द्र स्वामी जी की समाधि के कारण जैसे 'शिरडी' में सन्त श्री साई बाबा का समाधि स्थान है वैसे ही अति प्रसिद्धि प्राप्त स्थान है तथा शान्त, एकान्त और पूजादि धार्मिक कृत्यों-अनुष्ठानों के लिए सर्वोचित सात्त्विक वातावरण है। अब वह और भी अधिक अन्तर्मुखी हो गये। सदा भगवन्नाम गुनगुनाने में संलग्न रहते। न तो उन्हें वस्त्र की चिन्ता थी और न व्यवहार की। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। वह अपने कुल देवता वेंकटेश्वर तथा अपने इष्टदेव श्री राम की पूरा में तल्लीन रहते थे। वह बेला वाद्य पर लम्बे समय तक भजन गाते और रात्रि में देर से सोते थे। वह बाह्य शौच में इतना अधिक सावधान रहने लगे कि अपने वस्त्रों को किसी को स्पर्श तक नहीं करने देते थे। कभी-कभी वह श्रीधर को पूजा-कक्ष में प्रवेश करने तथा अपनी ओर से वैसी पूजा करने के लिए कहते थे। वह जानते थे कि श्रीधर का जन्म घरबार में आसक्त रहने के लिए नहीं हुआ है। वह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिसने वर्षों पश्चात् जब श्रीधर ने बहुत ही समृद्ध सांसारिक जीवन का त्याग किया तो कोई आश्चर्य तथा असन्तोष नहीं व्यक्त किया। पिता तथा पुत्र में ऐसा सद्भाव था। ऐसा प्रतीत होता है कि निष्ठावान् पुत्र ने राम-नाम को सूक्ष्म संस्कारों के रूप में अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था।
श्रीधर की शिक्षा का अन्तराल अल्पकालिक था। मातामह एन. वेंकट राव तथा मातामही सुन्दरम्मा देवी को बच्चों की शिक्षा की ओर श्रीनिवास राव की उदासीनता पर चिन्ता हुई और वे बच्चों को एक बार पुन. मंगुलूरु भेजने के लिए श्रीनिवास राव को सम्मत करने में सफल हुए। इस भाँति श्रीधर ने रोज़रियो में अपनी आद्य विहार-शिक्षा पुनः प्रारम्भ कर दी जहाँ उन्हें अब पाँचवीं कक्षा में प्रवेश मिला। यहाँ उन्होंने अनुभवी अध्यापकों की स्नेहशील देख-रेख में तृतीय वर्ग (अष्टम कक्षा) तक अध्ययन किया। इन अध्यापकों में से अधिकांश ईसाई पादरी थे। इस समय श्रीधर को भगवान् की खोज द्वारा हृदय की सान्त्वना की तलाश की प्रबल अन्तश्चालना अनुभव होने लगी। यहाँ रोज़रियो माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने तृतीय वर्ग तक की अपनी शिक्षा पूरी कर ली। इसके पश्चात् उन्होंने सेण्ट एलोसियस महाविद्यालय के उच्च विद्यालय विभाग में प्रवेश लिया जहाँ उन्होंने चतुर्थ (नवम कक्षा) तक अध्ययन किया जिसमें संस्कृत इनका एक वैकल्पिक विषय था।
इसी समय इनके मातामह के मित्र विठ्ठल राव ने, जिन्होंने सरस्वती मुद्रणालय की स्थापना की थी, एक उत्कृष्ट पुस्तक 'भगवान् की खोज में' का विमोचन किया जो सन्त रामदास की प्रथम कृति थी। पुस्तक भगवान् के उपहार के रूप में श्रीधर के हाथ लगी। विट्ठल राव ने पुस्तक की एक प्रति अपने मित्र एन. वेंकट राव को सम्मानार्थ प्रेषित की जो अपने-आप श्रीधर के हाथों तक पहुँच गयी। इसका आवरण सुन्दर हरे रंग का था। श्रीधर को अपनी स्वच्छ आलमारी में उसका रूप-रंग बहुत रुचिकर लगता था। उन्होंने इसका परिशीलन इतनी बार किया कि उनके मन में प्राय: सम्पूर्ण पुस्तक आलोक-लेख की भाँति अंकित हो गयी। इस पुस्तक के अध्ययन के समय यह केवल बारह वर्ष के किशोर बालक थे। जब उन्हें 'भाव-समाधि', 'गुह्य नेत्र' जैसे धार्मिक शब्द मिलते तो वह शब्दकोश की सहायता लेते और तब उनके आशय पर विचार करते। इन शब्दों में से कुछ के लिए उनमें विशेष रुचि उत्पन्न हो गयी। वह उनके गूढ़तम अर्थ की खोज का प्रयत्न करते। उनके लिए पुस्तक के प्रथम आकर्षणों में से एक उन तीर्थस्थलों का विवरण था जिनकी रामदास ने भगवान् की खोज में यात्राएँ की थीं। इस प्रकार, प्रारम्भ में यात्रा-विवरण के रूप में इस पुस्तक ने इनके चित्त को आकर्षित किया। धीरे-धीरे उनके हृदय की तन्त्री झंकृत हो उठी। उन्होंने इस पुस्तक की आध्यात्मिक धारा पर बहुत ही उत्साह तथा आनन्द की प्रतिक्रिया दिखलायी। हिमालय, गंगा तथा ऋषिकेश अब न केवल परिचित स्थान थे, वरन् ये उनके मन में बार-बार मँडराने लगे थे। रामदास की आध्यात्मिक आत्मकथा ने उन्हें कई दिनों तथा महीनों तक आनन्दातिरेक में रखा। जहाँ-कहीं भी वे जाते यह पुस्तक उनकी सहचर होती। "हे राम! आप ही पिता, माता, भ्राता, मित्र, गुरु, ज्ञान, यश, धन तथा सर्वस्व हैं। आप एकमात्र शरण हैं। अपने दास को सदा के लिए अपने में, एकमात्र अपने में ही विलीन कर लें।" सन्त रामदास के इस प्रकार के भक्तिपूर्ण भावोद्गार उनके हृदय को दिव्य प्रेमोन्माद से प्रभारित करते थे। इनकी भगवान् तथा ईश-मानव के प्रति उत्कण्ठा दिन-प्रति-दिन बढ़ती गयी।
श्रीधर को सन् १९३२ में मंगुलूरु तथा अपने बालकपन के मित्रों से विदायी लेनी पड़ी तथा नगर के बाह्यांचल जो अब शिनॉयनगर के नाम से प्रसिद्ध है, में 'किम्बली' कोठी में अपने पिता के साथ रहने के लिए चेन्नै को प्रस्थान करना पड़ा। यहाँ उन्हें सर एम. सी. टी. मुत्तैया चेट्टियार उच्च विद्यालय में प्रवेश मिला जहाँ उन्होंने दो वर्ष तक अध्ययन कर एस. एस. एल. सी. पाठ्यक्रम समाप्त किया। इस विद्यालय में उनके सहपाठियों में श्री ए. रामदास, श्री वी. आर. चक्रवर्ती, श्री एम. सुब्रह्मण्यम तथा कुछ अन्य लोग थे जिन्होंने भविष्य में जीवन के विभिन्न व्यवसायों में प्रतिष्ठा प्राप्त की। तथापि श्रीधर सर्वथा भिन्न साँचे में ढले थे। जन्म, शिक्षा, लालन-पालन, साहचर्य तथा स्वभाव से वह आध्यात्मिक जीवन की ओर हात् खिंच रहे थे। उनके सहपाठी उन्हें अधिकांश समय मौन तथा अन्तर्मुखी पाते। समय-समय पर के उनके सौम्य परिहास भी, जो उन्हें हास्य भाव में रखते, वास्तव में उनके सहपाठियों की इस भावना को कभी भी दूर नहीं कर पाये कि वह उनसे कुछ-कुछ भिन्न हैं। निस्सन्देह वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे तथा अपने विषयों पर सुगमता से अधिकार प्राप्त कर लेते थे। परन्तु वह कभी भी जीविका की दौड़ में लगे प्रतीत नहीं होते थे। उनकी समग्र सत्ता आध्यात्मिक स्पन्दनों से इतनी अभिभूत थी कि उनके अनेक मित्रों को ऐसा प्रतीत होता कि कक्षा में जो-कुछ होता, उसकी ओर वह कभी भी बहुत उत्सुक अथवा सावधान नहीं रहते थे। शैक्षिक उत्कर्ष की ओर उनकी उदासीनता के बावजूद भी उनका मन स्वभावतः एकाग्र होने से वह पाठ्य-विषयों को इतनी अल्पावधि में स्मरण कर सकते थे कि वह सदा ही मुत्तैया चेट्टियार उच्च विद्यालय के लब्ध-प्रतिष्ठ छात्रों में से एक माने जाते थे। वह अपने अध्यापकों से केवल पुस्तकों के पाठ सीखने के अतिरिक्त अनेक अन्य बातें सीख रहे थे। उन्होंने अपने अध्यापकों में से कुछ के समर्पित जीवन तथा गौरवपूर्ण आचरण से चरित्र के चिरस्थायी पाठ आत्मसात् किये। उनमें से कुछ अध्यापक परम्परानिष्ठ ब्राह्मण तथा श्री रामानुजाचार्य के वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे। प्रधानाध्यापक श्री तिरुवेंगलाचार्य, इतिहास के अध्यापक श्री सुन्दर राघवाचार्य, संस्कृत के अध्यापक श्री कृष्णमाचार्य तथा अँगरेजी के अध्यापक श्री गोविन्दाचार्य के भव्य तथा गौरवपूर्ण जीवन ने श्रीधर के हृदय पर अपना चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है। इन सबको स्वामी जी आज भी स्मरण करते हैं।
जब कि इनके सहपाठी इन्हें उदासीन तथा खोया-खोया रहने वाला साथी समझते, उस समय भी यह शान्तिपूर्वक उस ज्ञान की खोज में रहते जिसे एक बार जान लेने पर कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। अन्ततः शिक्षा मात्र एक प्रक्रिया है जो उस पूर्णता को प्रकट करती है जो व्यक्ति के अन्दर पहले से ही विद्यमान है। श्रीधर शान्तिपूर्वक उस पूर्णता को अभिव्यक्त करने का संघर्ष कर रहे थे जिसे उन्होंने अपनी अन्तर्दृष्टि से उस समय अपने में पहले से ही विद्यमान अनुभव किया था। अतः उनकी शिक्षा विद्यालय की चहारदीवारी तक ही सीमित नहीं थी। कुछ ऐसा था जिसमें वह सदा घर में, विद्यालय में तथा जहाँ-कहीं भी होते अपने को संलग्न रखते । श्रीधर के सहपाठी डा. रामदास उन्हें इस प्रकार स्मरण करते हैं: "एक सहाध्यायी के रूप में वह हम लोगों की तरह ही जीवन के आनन्द से पूर्ण थे। उन्हें क्रिकेट में वैसी ही बहुत रुचि थी, जैसी कि मुझमें थी। हम दो प्रतिद्वन्द्वी क्रिकेट टीमों के खिलाड़ी थे तथा प्रायः एक-दूसरे का सामना करने के लिए खड़े किये जाते थे। उनके माता-पिता किम्बलीं नामक एक असम्बद्ध पुरानी हवेली में अमिंजिकरै में रहते थे। यह स्थान चेन्नै के दक्षिण पश्चिम बाह्यांचल में था और अब यह महानगरीय चेन्नै का हलचल-पूर्ण स्थान है। उनके परिवार के लोग उदार थे और हमें अपने बड़े आहाते में क्रिकेट का मैच खेलने देते। महाराज स्वयं घर की पाकशाला से हमें अल्पाहार दिया करते थे।
"तथापि, उनमें और हममें एक अन्तर था। वह मधुरभाषी तथा भद्र थे। वह असत्य-भाषण करने, झगड़ने तथा अपने अध्यापकों से शरारत करने जैसे विपथगमन में कभी भी निरत नहीं होते थे जैसा कि उस आयु के सामान्य छात्रों से अपेक्षा की जाती है। कभी-कभी वह हमसे अध्यात्म की चर्चा किया करते। हमारे लिए यह भाषा विलक्षण थी और हममें से कुछ उन्हें सनकी समझने की भूल करते थे।" वर्षों बाद जब श्रीधर एक अत्यन्त पूजित आध्यात्मिक व्यक्ति थे, विश्वभर में सम्मानित तथा अभ्याकांक्षित व्यक्ति थे, वे अपने इस पुराने सहाध्यायी से उसी स्नेह से मिले जैसा कोई मिलनसार व्यक्ति अपने सन्मित्र के साथ प्रदर्शित करता है। किन्तु डा. रामदास अपने पुराने मित्र द्वारा उस समय विकीर्ण की हुई आत्मदीप्ति से अभिभूत हो उठे। उन्होंने एक क्षण में यह गम्भीरता से अनुभव किया कि वह एक भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त आत्मा के सान्निध्य में हैं।
निर्विकार तथा प्रशान्त प्रकृति से सम्पन्न श्रीधर स्वभावत: ही घर में अग्रजों के भी प्रेरणा-स्रोत थे। स्वामी वेंकटेशानन्द के शब्दों में, "श्रीधर विद्यालय में छात्र तथा घर पर साधु थे। उनके ओष्ठों से कभी एक कर्णकटु शब्द अथवा अश्लील वचन बाहर न निकलता। जब उनके ज्येष्ठ फुफेरे भाई किन्हीं असावधान क्षणों में सदोष वचनों का प्रयोग करते तो वह उन्हें बहुत ही शिष्ट शब्दों में सुधार दिया करते थे। यह ठीक ही कहा गया है, प्रभात दिन का सूचक है। अपनी किशोरावस्था में भी दरिद्रों के प्रति उनर्क। उदारता उनकी सर्वाधिक सुविज्ञात विशिष्टता थी। मुत्तुमारी नामक एक वृद्धा भिखारिन थी जिसे श्रीधर प्रतिदिन भोजन कराया करते। उन्हें निजी व्यय के लिए जो धन दिया जाता उससे वह औषधियाँ खरीद कर रोगियों तथा निर्धनों में वितरित करते थे। सेवा करने के लिए नहीं वरन् निस्स्वार्थ सेवा के अनुपम आदर्श में विकसित होने के लिए उनका जन्म हुआ था। लोग वीभत्स तिरस्करणीय पशु की भाँति कुष्ठरोगियों से दूर रहते हैं; किन्तु कुष्ठियों की सेवा श्रीधर के लिए एक स्वैच्छिक तथा नैसर्गिक कार्य था। वह उनके व्रणों की मरहम-पट्टी करते, आक्रान्त भाग पर औषधि लगाते और खाने के लिए औषधि देते। इन उपेक्षित तथा परित्यक्त मानव-प्राणियों के लिए उनमें असीम करुणा थी। जब इनके फुफेरे भाई वेंकट राव, जो इनसे छह वर्ष ज्येष्ठ थे, ने बिना समझे ही इनसे पूछा कि वह किशोरावस्था में कुष्ठियों की सेवा में क्यों इतनी भावप्रवणता से संलग्न हैं तो श्रीधर के पास अत्यन्त सरल किन्तु निरुत्तर बना देने वाला उत्तर था : “क्योंकि कुष्ठी भी आप और मेरे जैसे ही हैं।”
बाल्यकाल से ही वह सेवा, भक्ति तथा ध्यान के अपूर्व संघात थे। स्वामी रामदास की 'भगवान् की खोज में' नामक पुस्तक जिसका उल्लेख इससे पूर्व किया जा चुका है, ने इन्हें भगवान् के लिए पागल-सा बना दिया। "हे राम ! रामदास को अपने लिए पागल बना दें। वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा न करे। आप ऐसे करुणामय हैं। आप ऐसे स्नेहमय हैं। हे प्रेम! हे करुणा! रामदास को पूर्णतया अपना बना लें।" भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त सन्त के ये वचन उनके अन्दर गहराई से प्रवेश कर गये थे और श्रीधर भगवान् की खोज में, परम सत्ता के स्वरूप की खोज में अहर्निश संलग्न रहने लग गये।
इस अवस्था में उन्हें एक ऐसे मैत्रीपूर्ण पथप्रदर्शक की आवश्यकता थी जिसे वह अपने विचारों तथा भावनाओं में भागीदार बना सकें। इसके लिए उनके फूफा श्री आर. कृष्ण राव ही उपयुक्त व्यक्ति थे। वह श्रीनिवास राव के परिवार के एक सदस्य थे। उनकी एकमात्र बहन गोपी बाई उनसे ही विवाहित र्थी। वह अपने बाह्य जीवन में गृहस्थ तथा अपनी आन्तर सत्ता में सन्त थे। वह भगवान् श्रीराम के परम भक्त थे। किसी को यह भी पता नहीं कि उन्होंने कितने करोड़ राम का दिव्य नाम अपनी नोटबुकों में चुपचाप लिख डाला था और अपने-आपमें गुनगुनाते रहे। उन्होंने अपने किशोर भतीजे श्रीधर को भगवत्प्राप्ति के लिए जपयोग की साधना अपनाने के लिए प्रेरित किया। छप्पन वर्षीय इस भागवत पुरुष ने अपने व्यवहार तथा उपदेश से इस भगवान् के किशोर बालक पर प्रभाव डाला जो पहले से ही महान् आध्यात्मिक संस्कार बहुत ही स्वाभाविक ढंग से प्रकट करता था। दोनों ही एक-दूसरे में आध्यात्मिक प्रेरणा के प्रवाह को बढ़ाते थे। इन दोनों का सम्मिलित जीवन मानो विधिविहित सत्संग था। ऐसे ही भाग्यशाली संग को उद्दिष्ट करके भगवान् ने गीता में कहा है: "निरन्तर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा मेरा गुण-कथन करते हुए ही सन्तुष्ट होते हैं और मुझमें निरन्तर रमण करते हैं।" फूफा तथा भतीजे ने अपने अन्य पारिवारिक दायित्वों तथा बन्धनों को विस्मृत नहीं किया, फिर भी वे एक ही व्यवसाय में संलग्न भाइयों की भाँति एक साथ पूजा करते तथा विविध शास्त्रों तथा सन्त रामलिंग स्वामी, तायुमानवर आदि सन्तों के प्रेरणादायी जीवनों को एक-दूसरे को पढ़ कर सुनाते। सायंकाल से अर्धरात्रि तक वे आध्यात्मिक चर्चाओं में संलग्न रहते तथा प्राचीन शास्त्रों में अन्तर्विष्ट गम्भीर सत्यों की थाह लेने का प्रयत्न करते।
इन बैठकों के दिनों में ही श्रीधर कृतसंकल्प थे कि यदि निर्विकल्प-समाधि की प्राप्ति ही वह लक्ष्य है जहाँ व्यक्ति परम सत्ता का साक्षात् दर्शन करता है तो यह उनकी एक दार्शनिक संकल्पना मात्र न रह कर एक जीवन्त अनुभव होगा। अब वह एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति की खोज में थे जिसके लिए सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक चेतना एक यथार्थता रही हो, जीवन का निरन्तर अनुभूत तथ्य रहा हो। उन्होंने अपने आदर्श को दक्षिणेश्वर के ईशमानव रामकृष्ण परमहंस में साकार पाया। उन्होंने महेन्द्रनाथ गुप्त द्वारा स्मरणीय रूप से लिखित उत्कृष्ट तथा रोमांचक पुस्तक 'श्री रामकृष्ण की वार्ता' का अध्ययन किया। आर. कृष्ण राव ने ही रामकृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व का अपने प्रिय भतीजे से परिचय कराया था। चिर-काल से अनुभव की जा रही आवश्यकता अब पूर्ति की ओर बढ़ रही थी। श्रीधर इस महान् पुस्तक के अध्ययन तथा चिन्तन में दिन-रात लगे रहते। अन्त में उन्हें इसमें किंचित् भी सन्देह न रहा कि आध्यात्मिक अनुभूति की उत्कृष्टता एक यथार्थता है जिसे परमहंस देव ने न केवल स्वयं अनुभव किया अपितु विश्व को दिखलाने के लिए उसे प्रदर्शित भी किया। 'श्री रामकृष्ण की वार्ता' का अध्ययन श्रीधर के लिए केवल स्वाध्याय न रह कर सविकल्प-समाधि-सा था। उन्हें यह पूर्ण निश्चय हो गया था कि गदाधर विष्णु ने अपने भक्तों को दिये हुए वचन को पूरा करने के लिए स्वयं ही दक्षिणेश्वर के सन्त के रूप में अवतार लिया है। वह वार्ता को आद्योपान्त इतनी बार पढ़ गये कि वह उन्हें प्रायः कण्ठस्थ हो गयी। श्री रामकृष्ण देव के माता शारदामणि देवी के साथ असाधारण सम्बन्ध के अध्ययन से उनमें सामान्य रूप से स्त्री-जाति के प्रति एक मूलतः नवीन स्वरूप विकसित हुआ। वह प्रत्येक स्त्री में भगवती माँ के रूप को देखते थे। नवयौवन काल में स्त्रियों के सम्बन्ध में उनके इतने श्रद्धामय तथा निरपवाद शुद्ध विचार तथा व्यवहार को देख कर उनके मित्रों को आश्चर्य होता था। उनके लिए स्त्री भगवती माता की अभिव्यक्ति थी, इतना ही नहीं वह स्वयं नारायण की अलिंग आत्मा थी। वह रामकृष्ण की काली माता की पूजा से इतना अधिक प्रभावित थे कि एक समय वह अपने गृह-परिसर में भगवती माता का मन्दिर निर्माण कराना चाहते थे। अपने नवयुवक भतीजे के अन्दर जो निवृत्ति का पौधा प्रस्फुटित हो रहा था, उसे आर. कृष्ण राव ने ही उस समय सींचा तथा परिपोषण किया। उनके लिए श्रीधर को यह निश्चय कराना सरल था कि त्रिकाल में एकमात्र भगवान् ही सत्य हैं तथा अन्य सभी कुछ क्षणभंगुर है। अब केवल इस प्रकार के विचारों को निरन्तर प्रोत्साहित कर तथा सभी सम्भाव्य बाह्य विक्षेपों को भीतर आने से रोक कर उसे एक धारा के प्रवाह के रूप में निरापद बनाये रखना ही शेष रहा था। श्रीधर में कृष्ण राव के प्रति इतना सम्मान था कि चिर-काल पश्चात् सन् १९५० में जब वह प्रसिद्ध अखिल भारत यात्रा-काल में स्वामी शिवानन्द के साथ चेन्नै पहुँचे तो उस समय यद्यपि वह उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर चुके थे और संन्यासी बन चुके थे, फिर भी वह पुष्प तथा फल ले कर कृष्ण राव को मिलने को ऐसे भागे जैसे कि किसी सन्त से मिल रहे हों तथा अपने वृद्ध फूफा के चरणों में गम्भीर श्रद्धा तथा कृतज्ञता से साष्टांग प्रणाम किया।
अब किम्बर्ली में भगवान् श्री रामकृष्ण परमहंस देव श्रीधर के उपास्य थे। यह रामकृष्ण तथा शारदामणि के चित्र ले आये तथा सभी विहित विधि-विधानों का पालन करते हुए परम्परागत रीति से उनकी पूजा करने लगे। प्रत्येक रविवार को वह मैलापूर, चेन्नै के रामकृष्ण मिशन में जाते तथा रामकृष्ण की स्तुति में संस्कृत के मंजुल स्तोत्र सुनाते। उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के सम्पूर्ण साहित्य में उनके ओजस्वी भाषणों को पढ़ा जिसने उन्हें अध्यात्म की प्रबल विद्युत्-धारा से प्रभारित कर दिया। स्वामी विवेकानन्द का आधुनिक भारत का भावोत्तेजक आह्वान उनके लिए दैनिक गीता बन गया।
रामकृष्ण के उदार समन्वय-योग के साथ-साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वर-माधुर्य ने अब श्रीधर को सम्मोहित किया जो कि स्वाभाविक ही था, क्योंकि इनके माता-पिता तथा पूर्वज सभी श्री मध्वाचार्य-सम्प्रदाय के अनुयायी रहे थे। महान् वैष्णवाचार्य मध्व ने उड़ीपी में आठ मठ स्थापित किये थे। श्री मध्व के उत्तराधिकारियों के एक आनुषंगिक आम्नाय ने हास्पेट में उत्तराधि मठ की स्थापना की थी। उत्तराधि मठ के धर्माध्यक्ष परम पावन श्री स्वामी सत्यध्यान तीर्थ श्रीनिवास राव के परिवार के गुरु थे। वह महान् तपस्वी, ज्ञानी तथा सिद्ध थे। अपनी तपस्या तथा भगवती देवी की कृपा से वह देवी के कुंकुम को प्रसाद-रूप में वितरणार्थ द्रव्य-रूप में प्रकट कर दिया करते थे। जब वह राव जी के घर पधारे तो श्रीधर ने धर्माध्यक्ष के परम सन्तोषप्रद ढंग से उनकी स्वयं सेवा की और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी सत्यध्यान तीर्थ ने श्रीधर के शरीर पर शंख तथा चक्र की मुद्राएँ अंकित कीं।

श्री आर कृष्ण राव फूफा जी

लोकातीत दृष्टि -स्वामी जी
उनकी वैष्णव-कुल-परम्परा उन्हें चैतन्य गौड़ीय मिशन ले गयी। वह सप्ताह में एक बार चेन्नै के गौड़ीय मठ जाते और उनकी पूजा-पद्धति का पालन करते। वह वैष्णव देवगणों के धर्मात्मा पुरुषों के चरणों में दीर्घ दण्डवत् प्रणाम करते। इस दण्डवत्-प्रणाली ने, जो गौड़ीय मिशन की एक विशिष्टता है, श्रीधर का हार्दिक अनुमोदन प्राप्त किया। इससे उन्हें व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में विनम्रता तथा अनात्मशंसा की परम महत्ता समझ में आयी। गुरुदेव शिवानन्द इस प्रकार की विनम्रता का अभ्यास पास करते थे तथा इस प्रकार की नमस्कार-साधना को अहं के मिटाने की उपयोगी विधि के रूप में प्रदिष्ट करते थे। विनम्रता आध्यात्मिक साधक का प्रथम गुण है। उसे सदा इस दिव्य गुण का सम्पोषण करने के लिए उत्कण्ठित रहना चाहिए। यही कारण है कि दण्डवत्-प्रणाली-जैसी प्रतीयमानतः सामान्य-सी वस्तु श्रीधर जैसे वास्तविक साधक में महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना में रूपान्तरित हो गयी।
इस प्रकार छोटी-बड़ी साधनाओं के द्वारा श्रीधर जब आध्यात्मिक शिक्षा में अनभिव्यक्त रूप से प्रवीणता की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय सन् १९३४ में उन्होंने उच्च विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात् उन्होंने लोयोला महाविद्यालय में प्रवेश लिया जिसमें इण्टरमीडिएट (कला) में इतिहास तथा तर्कशास्त्र और बाद में स्नातक (कला) में इतिहास तथा अर्थशास्त्र उनके अतिरिक्त विषय थे। महाविद्यालय में आने के बाद वह स्वभाव से और भी अधिक अन्तर्मुखी तथा चिन्तनशील बन गये। वह प्रतिदिन दीर्घकाल तक सन्त-सम्बन्धी पुस्तकों के अध्ययन करने, सामान्य जीवन पर चिन्तन करने तथा आध्यात्मिक साधनाएँ करने में व्यस्त रहते। ऐसी धर्माभिमुखता होते हुए भी, उन्होंने अपना पाठ भली-भाँति पढ़ा तथा इण्टर की परीक्षा गौरव के साथ उत्तीर्ण की। उनकी अन्तर्मुखी तथा अर्ध रहस्यमयी जीवनचर्या ने उन्हें अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों से अप्रभावनीय नहीं बनाया। वह बहुत ही समाजमूलक उत्साह प्रदर्शित करते थे तथा जीवन से अत्यधिक प्रेम करते प्रतीत होते थे। अपने सुन्दर कटे घने बालों, कौशेय वस्त्रों से आवृत लम्बे आकार तथा आपीत-रक्त कान्ति से आप्लावित मनोरम आकृति से वह सदा समागमों में लोगों के ध्यान के केन्द्र बनते। इस भूषाचारी रूप-रंग तथा आधुनिक शैक्षिक जीवन की प्रवृत्ति के बावजूद भी इनका जीवनविषयक दृष्टिकोण अत्यधिक आध्यात्मिक ही बना रहा। वह प्रायः चिन्तनशील दिखायी पड़ते तथा कक्षा से जहाँ वह बैठे होते, बहुत दूर स्थित रहते। अधिकांश अन्य लोगों की भाँति उनके मन में धार्मिक विचार अन्य सैकड़ों सांसारिक विचारों के साथ केवल सभामंच के अवसर पर समय-समय उद्धृत करने के लिए ही नहीं मँडराया करते थे। वे तो उनकी आत्मा के अत्यधिक प्रिय आहार थे। वे उन पर घण्टों चिन्तन करते और उनके अनुसार अपना जीवन निर्देशित करने के लिए नैतिक मान्यताओं के रूप में उन्हें अपनी सत्ता के अन्तर्तम प्रकोष्ठ में सँजोये रखते। इनकी मूल सिद्धान्तों में गम्भीर निष्ठा तथा उन पर अटल बल स्वभावतः ही इनके मित्रों के लिए कभी-कभी आश्चर्यकर वस्तु बन जाते। उदाहरणतः एक दिन जब उनके मित्रों के मध्य कुछ कृत्रिम दार्शनिक चर्चा सामान्य तरुणसुलभ जोश से चल रही थी, श्रीधर अकस्मात् ही वी. आर. चक्रवतों की ओर अभिमुख हुए और पूछा, 'आपका' मैं तथा 'आप' शब्दों से क्या तात्पर्य है? आपका तात्पर्य शरीर से है अथवा आत्मा से? ऊँचे स्वर से आ रही आवाज तुरन्त शान्त पड़ गयी। जो छात्र आंशिक रूप से आत्मसात् किये हुए तथा दूसरों से गृहीत दार्शनिक विचारों की सोत्साह चर्चा आध घण्टा अथवा इससे अधिक समय से चला रहे थे, अब सहसा मौन तथा संकोचित हो गये; क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि श्रीधर के सरल प्रश्न तथा शान्त किन्तु गम्भीर आचरण के सामने कैसे आगे बढ़ें।
लोयोला महाविद्यालय का छात्र-जीवन उन्हें ईसाई धर्म के घनिष्ट सम्पर्क में लाया। पवित्र बाइबिल ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। अन्य ईसाई लेखक टोमस ए. केम्पिस कृत 'इमिटेशन आव् क्राइस्ट' ने उनके मन पर अमिट प्रभाव छोड़ा। क्रूस पर अभिनीत महाबलिदान में उन्हें निम्न आत्मा के प्रति मरने तथा शाश्वत जीवन के लिए जीने के सन्देश की अभिव्यंजना मिली। असीसी के सन्त फ्रांसिस ने, जो भगवान् के सभी प्राणियों के, विशेषकर पक्षियों तथा अबोध पशुओं के प्रति अपनी असीम करुणा के लिए विख्यात थे, श्रीधर पर इतना शक्तिशाली प्रभाव डाला कि वह पबित्र सन्त की आत्मा के साथ एकत्व की अनुभूति करने लगे। सन्त फ्रांसिस की इस प्रार्थना को उन्होंने प्रायः गुरुमन्त्र के रूप में स्वीकार किया :
बना निज शान्तिदूत हे ईश !
जहाँ घृणा हो प्यार को बोऊँ;
हिंसास्थल पर क्षमा सँजोऊँ;
फूटपृथकता प्रेम से जोहूँ;
शक को अपनेपन में मोहूँ;
जहाँ निराशा आशा भर दूँ;
तम में जगमग ज्योति कर दूँ;
हर्ष भरूँ मैं दुःख विषाद में, हे मेरे जगदीश ।
बना निज शान्तिदूत हे ईश ।।
दिव्य आत्मन्। परम आत्मन् ! कर यह बुद्धि प्रदान।
तुष्टि लेने से ज्यादा मैं, करूँ सान्त्वना दान ।
ज्ञानी समझा जाने से, अच्छा मैं समाँ ज्ञान।
प्यार किये जाने से समहूँ, करना स्नेह महान्।
निहित सदा देने में पाना, क्षमित से क्षमा प्रदान ।
क्योंकि मरण में छिपी अमरता, यह है फ्रांसिस का उद्गान!

लोयोला कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में

किम्बर्ली भवन
बाद में, उन्होंने इसका मूल्यांकन कर इसे अपने गुरुदेव स्वामी शिवानन्द की उत्कृष्ट 'विश्व-प्रार्थना' के तुल्य माना।
लोयोला महाविद्यालय के अपने आवास-काल में श्रीधर ने अपनी शान्त, प्रफुल्ल तथा विनोदशील मनोवृत्ति द्वारा विशिष्टता प्राप्त की। उनका आध्यात्मिक बोध किसी अस्थाई गुदगुदाहट अथवा क्षणभंगुर उत्तेजना का परिणाम न था। उनकी दृढ़ निष्ठा, उनके सामाजिक व्यक्तित्व को बिना किसी प्रकार के असन्तुलन में डाले हुए उनकी सत्ता में सामंजस्यपूर्ण ढंग से संघटित थी। आध्यात्मिक उन्नति में प्रवृत्त रहने पर उन्होंने अपनी शारीरिक उन्नति की उपेक्षा नहीं की। यह इस विषय से पूर्णतया अवगत थे कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर एक पूर्वापेक्षा है। यहाँ यह जानना रुचिकर होगा कि इस अवधि में इस बाल-प्रौढ़ आध्यात्मिक साधक में किम्बली क्रिकेट क्लब नामक क्रीड़ा-संघ को संघटित करने की अन्तश्चालना तथा क्षमता दोनों ही थीं। क्लब का नामकरण चेन्नै में पारिवारिक कोठी के हाते के नाम पर किया गया। क्लब के सदस्य बहुत उत्साही तथा नियमित खिलाड़ी थे। यह एक रोचक बात है कि गृहत्याग के पश्चात् भी, जब श्रीधर शिवानन्द-आश्रम के अन्तेवासी साधक थे, तब भी वह क्रिकेट खेलना अनुचित नहीं समझते थे। वह कुशल तैराक थे तथा 'मनोहर-विलास' के अहाते में स्थित तालाब में दूर तक तैरने में आनन्द लेते थे। वह निश्चय ही सर्वांगीण जीवन-यापन करते थे। एक ओर तो वह जहाँ अपराह्न में अतिस्पृहा के साथ क्रिकेट खेलते, वहीं दूसरी ओर प्रात:काल को योगासनों में लगाया करते थे।
शारीरिक संवर्धन तथा आध्यात्मिक साधना के इस व्यापक कार्यक्रम के साथ-साथ श्रीधर धार्मिक आचरण-सम्बन्धी कुछ मूलभूत सद्गुणों के सम्पोषण में भी अध्यवसायी थे। इस भाँति विकसित हो कर वह उदात्तता, प्रशान्ति तथा औदार्य के मूर्तरूप बन गये। वह सदा ही निर्धनों, रुग्णों, निराश्रयों, उपेक्षितों तथा दलितों की सेवा करने के अवसर की ताक में रहा करते थे।'[5] उनकी सेवा तथा सद्भाव के इस प्रेम में मूक पक्षियों तथा पशुओं का भी समावेश था। इस कालावधि में वह मैलापूर के रामकृष्णा मिशन की युवक-वाहिनी के एक सदस्य के रूप में निस्स्वार्थ सेवा में अपने को संलम रखते। सभी चर तथा प्राणधारियों के लिए प्रेम तथा उनकी सेवा उनका एक साहजिक तथा अनवरत व्यसन था। जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा के दर्शन करता है, उसमें 'मैं' तथा 'मेरा' की भावना नहीं रहती; अत: वह भगवान् के विराट् स्वरूप में भगवान् के रूप में सभी प्राणियों की सेवा करता है। कुष्ठरोगियों तथा रोगग्रस्त प्राणियों तथा भटकने वाले कुत्तों की सेवा उनके दैनिक कार्यक्रम का अंग बन गयी । एक बार उन्होंने चेचक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति की दीर्घकाल तक सेवा की जिसके कारण वह स्वयं चेचक से बीमार पड़ गये। इससे उन्हें न तो कोई पश्चात्ताप हुआ और न कोई भय ही। उन्होंने अक्षुण्ण उत्साह से सेवा चालू रखी। प्रयोजन तथा उत्प्रेरणा पूर्णतया निस्स्वार्थ थे; अतः उनके लिए जो भी वैयक्तिक कष्ट झेलने पड़ते, वे उनके समुत्साह को कभी भी अवमन्दित नहीं किये। अब श्रीधर फादर डैमियन की भाँति समर्पित जीवन-यापन कर रहे थे। वह उन कुष्ठियों को अपनी स्नेहशील, श्रद्धामयी सेवा अर्पित करते थे जिनसे संसार घृणा तथा सन्त्रास से मुख मोड़ लेता है। इनके गुरु शिवानन्द के विषय में एक बात थी कि इस प्रकार की दीर्घकालिक निस्स्वार्थ सेवा ने, संन्यास-जीवन में प्रवेश करने से बहुत पूर्व ही उन्हें व्यावहारिक वेदान्ती बना दिया।
एक ऐसा समय आया जब सद्भाव तथा सेवा का यह महान् व्यसन भी मोक्ष की ज्वलन्त कामना की तुलना में बाह्य अंग-सा प्रतीत होने लगा। परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए त्याग के मार्ग पर चलने तथा सभी दुःखों की निवृत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति की अवस्था प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले महान् ऋषियों का वज्रनिर्घोष आह्वान उनकी आत्मा में प्रतिध्वनित होने लगा जिसने अन्य सारी भावनाओं को अभिभूत कर दिया। उन्हें यह मालूम था कि अनासक्ति का पोषण महापुरुषों में आसक्ति से होता है। अतएव, वह अपनी किशोर अवस्था से ही मनीषीजनों की संगति में अध्यवसायपूर्वक लगे रहते थे। उन्हें यह महत् जनों की सगति प्रमातामह सहचारी वेंकट राव तथा फूफा आर. कृष्ण राव से -जो स्वयं भगवत्साक्षात्कार से सम्पन्न महान् भक्त थे-घर पर ही प्राप्त करने का सद्भाग्य मिला। बाल्यकाल में व्रजेश्वरी के महान् सिद्ध स्वामी नित्यानन्द के आकस्मिक दर्शन मात्र से इनके सात्त्विक मन पर महान् आध्यात्मिक छाप पड़ी। भगवान् की खोज के सन् १९३२ से सन् १९४० तक के इन नौ महत्त्वपूर्ण वर्षों में श्रीधर की आध्यात्मिक आकांक्षा निरन्तर उत्थान की ओर थी। जब वह चेन्नै के मुत्तैया चेट्टियार उच्च विद्यालय में षोडश वर्षीय एक किशोर छात्र थे, तभी से उन्होंने सुप्रतिष्ठित सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों तथा भक्तों के साथ अपना सम्पर्क बनाये रखा। अल्मोड़ा के श्यामल-ताल के श्री स्वामी विरजानन्द के मद्रास में आगमन का श्रीधर पर स्मरणीय प्रभाव पड़ा। श्रीधर के सम्मुख हिमालय के यह महान् सन्त उत्तराखण्ड के ऋषियों के उन सभी आध्यात्मिक गुणों के सच्चे मूर्तरूप में दिखायी पड़े जिन्हें उन्होंने अपने बाल्यकाल के प्रारम्भिक दिनों में अपनी माता से सुन रखा था। इस भेंट से उनमें हिमालय जाने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई।
परवर्ती सन् १९३२ में किसी समय इन्होंने समाचार पत्रों में श्री पुरोहित स्वामी के चेन्नै आगमन का समाचार पढ़ा। श्री पुरोहित स्वामी गैरिक परिधानधारी भिक्षु न होते हुए भी एक रहस्यवादी योगी थे। वह एक परिव्राजक तपस्वी तथा भगवान् दत्तात्रेय के उपासक थे। उन्हें नादयोग में महान् सिद्धियाँ प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त था। उन्होंने प्राच्य तथा पाश्चात्य जगत् के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर अपना गम्भीर प्रभाव छोड़ा था। श्रीधर को इस लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति के विषय में प्रकाशित कुछ लेखों से पहले ही उनका परिचय मिल गया था। समाचार-पत्रों से यह जान कर कि पुरोहित स्वामी मद्रास विश्वविद्यालय में भाषण देने वाले हैं, वह तीव्र प्रत्याशाओं के साथ वहाँ नियत समय पर पहुँच गये और भाषण के अन्त तक तल्लीन मनोयोग से बैठे रहे। वह भाषण से इतने अनुप्राणित हुए कि उन्होंने वह स्थान जहाँ सन्त ठहरे हुए थे, खोज निकाला और फल तथा पुष्प की भेंट ले कर उनसे मिलने गये। पुरोहित स्वामी जी ने श्रीधर की उन्नत चेतना को स्पष्ट रूप से देख लिया और उन्होंने उन्हें मूलभूत सिद्धान्तों की शिक्षा देने तथा उससे उपलब्ध होने वाले अनुभवों को समझाने के लिए इनके साथ कुछ समय व्यतीत किया । श्रीधर साधना की विविध अवस्थाओं में साधक के मन में उत्पन्न होने वाली वीणा, वंशी, किंकिणि तथा घण्टा जैसी अन्तर्ध्वनियों (अनहदनाद) की पुरोहित स्वामी की व्याख्या से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने निवृत्ति-मार्ग का अनुसरण करने का पहले से ही निर्णय ले रखा था। पुरोहित स्वामी के आशीर्वाद से उनका संकल्प दृढ़ हो गया। तदनन्तर चेन्नै में उन्हें एक अन्य महान् सन्त स्वामी गायत्र्यानन्द के दर्शन हुए तथा दिव्यानुभूति की खोज में अग्रसर होने के लिए उनसे आशीर्वाद तथा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ।
वह सन् १९३६ में श्री रमण महर्षि से अरुणाचलम् में उनके पवित्र आश्रम में मिले। तीन दिन तक श्री रमण के सान्निध्य में रह कर इन्होंने इस महान् आत्मा की मौन रूप में सौम्य कृपा प्राप्त की। इसी वर्ष वह सामान्यतया मलयाला स्वामी के नाम से विख्यात स्वामी असंगानन्द गिरि से मिले। मलयाला स्वामी ने श्रीधर को तिरुपति के निकट येरपेडु के व्यासाश्रम में दर्शन दिया था। इस मिलन से श्रीधर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा जो उन दिनों सांसारिक सुख-सुविधाओं तथा ऐहिक प्रतिफलों से उदासीन रह कर श्वेत वस्त्र में न्यूनाधिक सन्यासी जीवन-यापन कर रहे थे।
इसके पश्चात् वह श्री स्वामी राजेश्वरानन्द के सम्पर्क में आये जो चेन्नै के प्रख्यात सन्त, सच्चिदानन्द-संघ के संस्थापक तथा हमारे देश के एक लब्ध-प्रतिष्ठ दार्शनिक डा. टी. एम. पी. महादेवन के आध्यात्मिक उपदेशक थे। सन्त ने श्रीधर के यशस्कर भविष्य को अपने मानस-चक्षुओं से देख लिया और उन्हें आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित किया। श्रीधर के रामकृष्ण मठ में प्रायः जाते रहने से वह रामकृष्ण मिशन के श्री स्वामी अशेषानन्द के निकट सम्पर्क में आये। रामकृष्ण मिशन के इस लब्ध-प्रतिष्ठ संन्यासी ने अन्तर्ज्ञान से यह अनुभव किया कि श्रीधर एक दिन सन्त-जगत् में देदीप्यमान् मणि की भाँति चमकेंगे। अतएव वह श्रीधर के आध्यात्मिक विकास में विशेष रुचि लेते थे।
उन्हीं दिनों एक अन्य प्रख्यात सन्त जिनसे श्रीधर मिले, श्री स्वामी आनन्दाश्रम थे, जो श्री स्वामी रामदास के घनिष्ठ साथी थे। अन्त में सन् १९४० में वह स्वयं महान् रामदास से मिले जो कांजनगढ़ के आनन्दाश्रम के संस्थापक थे तथा जिन्हें उनके भक्त प्रेम से 'पापा' कहा करते थे। इन्हीं स्वामी रामदास की आत्मकथा ने श्रीधर को आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रथम प्रेरित किया था। इसके श्रद्धेय लेखक से इस अपरोक्ष सम्पर्क ने इन पर अविस्मरणीय प्रभाव डाला। प्रिय पापा किशोर बालक में मोक्ष की ज्वलन्त कामना देख कर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें सफल होने का आशीर्वाद दिया और स्नेह से इनकी पीठ थपथपायी। राम के इस सेवक के पवित्र संस्पर्श से श्रीधर दिव्य हर्षातिरेक से आपूरित हो गये।
इन पूतात्मा भागवतजनों के निकट सम्पर्क तथा इनके आशीर्वादों ने इन पर अप्रतिरोध्य प्रभाव डाला तथा आगे के महान् जीवन-लक्ष्य के लिए पार्थिव जीवन-वृत्ति के चुपचाप त्याग करने को इन्हें प्रेरित किया। रोगियों, निर्धनों तथा निराश्रितों की सेवा ने इनके मन को पवित्र बनाये रखा तथा इनके स्वाध्याय और ध्यान ने इन्हें धार्मिक उपासना के लिए तीव्र ग्रहणशील बना दिया था। अतः महात्माओं के उपदेश तथा उत्प्रेरणाएँ इनके मन के अन्तर्तम प्रदेश में गहराई से प्रवेश कर गये। वह अब उच्च आध्यात्मिक धरातल पर पहुँच गये थे। यद्यपि इनका पालन-पोषण प्राचुर्य तथा समृद्धि के मध्य हुआ था तथापि महान् तपस्या का जीवन अपनाने में इन्होंने असाधारण आत्मविश्वास तथा शान्ति प्रदर्शित किये। इन्होंने जूता पहनना त्याग दिया, कौशेय वस्त्रों को फेंक दिया तथा सादी धोती और साधारण-सी कमीज पहन ली और उन सभी विषयों से तीव्र उदासीनता रखने लगे जिनके लिए युवक लालायित रहते तथा जिनमें आनन्द लेते हैं। निवृत्ति की अभिवृत्ति अब उनके व्यक्तित्व में पूर्णतया सन्निविष्ट थी। उन्हें ऐसा लगा कि वह संसाराग्नि में झुलस रहे हैं। गंगा की शीतलता की ओर भागने के लिए उपयुक्त समय की उत्सुकता से प्रतीक्षा में थे। अब वह घर में ही अनभिव्यक्त रूप से चरम त्याग की तैयारी करते हुए एक योगी का जीवन-यापन कर रहे थे। सेवा, सत्संग तथा साधना- ये तीन कार्य ही उनके दैनिक जीवन की विशेषता थे। उन दिनों वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे जिसमें आध्यात्मिकता का पुट न हो। उदाहरणार्थ लगभग उन्हीं दिनों इन्होंने दो चलचित्र 'तुकाराम' तथा 'सन्त ज्ञानेश्वर' - देखे। महाराष्ट्र के इन दो महान् सन्तों के सेलूलायड जीवनों ने उन्हें सम्मोहित कर लिया। वह इनसे प्रायः मोहित थे। इन्हें वे बार-बार देखने गये और प्रत्येक बार अपने परिवार के किसी-न-किसी व्यक्ति को अपने साथ ले गये । उन्होंने तुकाराम के प्रायः सभी अभंग कण्ठस्थ कर लिये। इन्हें गम्भीर भाव से गुंजायमान स्वर में गाते समय वह भावसमाधि में चले जाया करते थे। उन्होंने एक तम्बूरा खरीद लिया और उसकी संगति में भक्तिपूर्ण गीत गाने का अभ्यास किया।
सन्त ज्ञानेश्वर के चलचित्र से वह कितनी मात्रा में प्रभावित हुए थे, यह एक प्रसंग के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। संन्यास-ग्रहण के अनेक वर्ष पश्चात् जब वह दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष भी बन चुके थे, अपने ४९ वें जन्म-दिवस के आगामी दिन अर्थात् २५ सितम्बर १९६५ को संयोगवश वह हरिद्वार में थे। अकस्मात् उन्होंने दो कारें ऋषिकेश के शिवानन्दाश्रम भेज कर स्वामी कृष्णानन्द, स्वामी माधवानन्द, स्वामी दयानन्द, स्वामी प्रेमानन्द तथा नरसिंहमुलु सहित लगभग दश आश्रमवासियों से एक महान् सन्त से मिलने के लिए हरिद्वार आने का अनुरोध किया। वे सब महात्मा से मिलने की उत्कण्ठापूर्ण प्रत्याशा से हरिद्वार आये। उन्हें तब विस्मय तथा संकोच हुआ जब स्वामी जी उन्हें एक चलचित्र-भवन में ले गये और बताया कि उनकी इच्छा है कि वे सब सन्त ज्ञानेश्वर से वहाँ मिलें। तभी वरिष्ठ आश्रमवासियों को निमन्त्रण के किंचित् विनोदशील स्वरूप का पता चला, किन्तु स्वामी जी इस विषय में पर्याप्त गम्भीर थे और उन्हें बताया कि वह अपने प्रारम्भिक जीवन में किस प्रकार इस चलचित्र से अनुप्राणित हुए थे। उन्होंने सोचा कि यही सर्वोत्तम वैयक्तिक भेंट है जो वह अपने जन्म-दिवस पर उन्हें अर्पित कर सकते हैं।
लोगों को महात्मा गान्धी की इस प्रकार की अनुभूति की स्मृति है। उन पर भी 'श्रवणकुमार' तथा 'हरिश्चन्द्र' नामक दो चलचित्रों का दूरगामी तथा स्मरणीय प्रभाव पड़ा था। इस भाँति मोहनदास एक ऐसी प्रक्रिया में दीक्षित हुए जिसकी अन्ततः चरम परिणति उनके महात्मापन में हुई। इसी भाँति श्रीधर भी दो चलचित्रों को देख कर दिव्य प्रेमोन्माद से अधिभारित हो गये तथा आध्यात्मिक धीर पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने की उनकी सुलगती हुई कामना अन्तःप्रेरणा की प्रचण्ड ज्वाला में एकाएक बढ़ चली जिसने आगे चल कर उन्हें अन्ततः कालातीत सत्ता में, चिदानन्द में रूपान्तरित कर दिया। कदाचित् अपने इस वैयक्तिक अनुभव के कारण ही स्वामी चिदानन्द आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए चित्रपट के माध्यम के उपयोग के पक्ष में हैं।
दो महान् सन्तों के जीवनों को चित्रपट पर देख कर श्रीधर ने अपने को दुष्कर साधना में संलग्न कर दिया। वह किम्बर्ली कोठी के सबसे ऊपरी भाग पर चढ़ जाते तथा वहाँ घण्टों ध्यान में बैठे रहते। इसी समय चेन्नै के श्री पी. के. विनायक मुदालियार द्वारा सम्पादित लोकप्रिय पत्रिका 'माई मैगजीन आव इण्डिया' में आध्यात्मिक साधकों के व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए शिवानन्द शृंखलाबद्ध लेख लिख रहे थे। श्रीधर लोयोला महाविद्यालय के समीप की दुकानों से यह पत्रिका खरीद लेते थे तथा गम्भीर ध्यान तथा उस पत्रिका में अंकित स्वामी शिवानन्द के अतिस्पृहणीय उपदेशों के अभ्यास में संलग्न रहते। तत्काल ही उन्होंने स्वामी जी की पुस्तक Yoga by Japa (जप द्वारा योग) की एक प्रति प्राप्त कर ली तथा प्रतिदिन घण्टों जप तथा ध्यान में निमग्न हो कर महायोगी के उपदेशों को अभ्यास में परिणत करते। बाद में गुरुदेव की दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकों अर्थात् Spiritual Lessons (आध्यात्विक, शिक्षावली) तथा Mind, Its Mysteries and Control (मन : रहस्य और निग्रह) से इन्हें और अधिक प्रेरणा मिली।
स्वामी जी की व्यावहारिक शिक्षाओं ने श्रीधर को ध्यान का उत्कृष्ट पथ प्रदान किया तथा वह उच्चतर साधना-जगत् में शीघ्र ही पाँव जमाने लगे। अब इस निरवद्य ब्रह्मचारी ने भगवत्प्राप्ति के अतिसंयमी तथा कठोर मार्ग के लिए अपना यौवन अर्पित कर दिया। इस पुण्यात्मा ने जिसका जीवन सदाचार का आदर्श था, अब अन्य सभी विचार तथा कार्य को छोड़ कर 'किम्बर्ली' के छज्जे पर गम्भीर साधना में अपने को तल्लीन कर दिया। ध्यान के प्रवेश-द्वार द्वारा वह आध्यात्मिकता के उच्चतर क्षेत्र में जितना अधिक प्रवेश किये, उतनी ही अधिक तीव्रता से उन्हें यह अनुभव होने लगा कि साधना में पूर्णकालिक तल्लीनता के लिए संन्यास परमावश्यक है। यह विलक्षण-सा लगेगा कि ईश्वरेच्छा की व्यवस्था से उनके नवयौवनकाल में भी उनके विवाह का प्रश्न कभी भी नहीं उठा। इस पूर्ण ब्रह्मचारी को अस्थायी रूप से भी संसार-पाश में आबद्ध नहीं होना था।
श्रीधर को अब कार्यसंकुल वातावरण से अरुचि हो गयी। वह अपनी मौसी मालती बाई से कहते, "यदि ईश्वर को विस्मरण करना चाहती हैं तो बेंगुलूरु चली जायें।" नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से उन्हें घृणा हो गयी। वह किसी आश्रम की नीरवता तथा एकान्त के लिए लालायित थे जिससे कि वह अपने को एकमात्र आन्तर आध्यात्मिक साधना में पूर्णतया लगा सकें। वह एक गुरु के लिए भी तृषित थे जो शुद्ध आध्यात्मिक जगत् में इनका पथप्रदर्शन करे। किन्तु घर में किसी को भी इनके मन के अपसरण का बोध न हो सका। इस प्रकार वह सन् १९३६ में जब इनकी इण्टरमीडिएट की परीक्षा बहुत ही निकट थी, एक दिन घर से अदृश्य हो गये जिससे इनके मित्रों तथा सम्बन्धियों को बहुत चिन्ता हुई तथा उन्हें आघात पहुँचा। घर के वयोवृद्ध लोग उनके सरल तथा कठोर जीवन, भोजन तथा वस्त्र के प्रति उनकी उदासीनता, भौतिक समृद्धि की उनकी उपेक्षा तथा स्वाभाविक विलगाव और चिन्तनशील मनोदशा से न्यूनाधिक रूप में अपना सामंजस्य स्थापित कर चुके थे; किन्तु किसी को यह पूर्वानुमान न था कि इस नवयुवक में इतना शीघ्र पूर्ण त्यागमय जीवन में छलाँग लगाने के लिए साहस तथा दृढ़ता है। वे बहुत ही उद्विग्म हुए तथा जोरदार खोज आरम्भ हुई। उनके आद्य उत्प्रेरक आर. कृष्ण राव भी उनके पलायन की योजना के विषय में सर्वथा अनभिज्ञ थे। उन्होंने अपने पुत्र वेंकट राव तथा भतीजे गोविन्द राव के साथ चतुर्दिक् पूछताछ की, किन्तु इस यशस्वी कर्तव्यपराङ्मुख व्यक्ति का कहीं पता न चला।
श्रीधर को भगवान् रमण के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। वह महर्षि के पवित्र चरणों की शरण लेने के लिए लुकछिप कर पूजार्ह अरुणाचलम् पहुँच गये। उन दिनों महर्षि सदा अन्तर्मुखी वृत्ति में रह रहे थे। वह अपनी अनिमेष दृष्टि को अनन्त की ओर रख कर सदा गम्भीर तथा शान्त रहते तथा अत्यावश्यक विषयों पर आश्रम के सेवकों से केवल बहुत ही कम शब्दों में बोलते थे। श्रीधर ने उनके पवित्र सान्निध्य में मौन आध्यात्मिक संवाद में तीन दिन व्यतीत किये। महर्षि ने अपने मौन द्वारा कुछ-कुछ यह सूचित कर दिया कि वह नियति द्वारा नियत गुरु नहीं हैं। ब्रह्माण्डीय योजना में गुरु तथा शिष्य का सम्बन्ध पूर्व-निर्धारित हुआ करता है। श्रीधर ने महर्षि के साथ तीन दिन के मौन संवाद के पश्चात् उन्नत किन्तु जीवन-पोत के जिस लंगर-स्थल की खोज में थे, उसको प्राप्त किये बिना ही अरुणाचलमम् से प्रस्थान किया। वह वापस नहीं लौटे।
वह अरुणाचलम् से तिरुपति के निकट येरपेडु में व्यासाश्रम, मलयाला स्वामी के रमणीक आश्रम की ओर आगे बढ़े। यही मलयाला स्वामी बाद में स्वामी असंगानन्द गिरि के नाम से विख्यात हुए। किन्तु स्थान बहुत दूर था और इनके पास एक भी पैसा न था। तथापि वह गन्तव्य तक पहुँचने के लिए कृतसंकल्प थे। इस प्रकार आने वाले अवश्यम्भावी सभी शारीरिक कष्टों की अवहेलना कर रेल की पटरी के साथ-साथ वह चलते रहे। एक घण्टा तक चलने के पश्चात् इस वैभवशाली नवयुवक को एक स्थान पर रुक कर एक किसान से, जो कुएँ से जल निकाल रहा था, भोजन माँगना पड़ा। किसान ने इन्हें थोड़ी दलिया दी। श्रीधर उसे निगल गये तथा किसान को भिक्षादान के लिए धन्यवाद दे कर पुनः चलना आरम्भ कर दिया। घण्टों तक चलते रहने के पश्चात् सभी उपलभ्य शक्ति के क्षीण हो जाने पर वह लड़खड़ाते हुए एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और प्लेटफार्म पर पड़े एक फलक के सहारे लेट गये। एक युवक स्टेशन मास्टर ने उन्हें देख लिया और उनका परिचय जानना चाहा। श्रीधर उस समय एक फकीर जैसे दिखायी पड़ते थे। उन्होंने जब स्टेशन मास्टर को प्रांजल तथा परिशुद्ध अँगरेजी में उत्तर दिया तो वह आश्चर्यचकित रह गया और उनमें अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की। श्रीधर की उपस्थिति से उस पर कुछ विलक्षण प्रभाव पड़ा और उसने युवक जिज्ञासु को कुछ आध्यात्मिक चर्चा में उलझाया। उसको महान् आश्चर्य तथा सन्तोष हुआ जब श्रीधर ने उसकी सभी शंकाओं को विदूरित कर दिया। स्टेशन मास्टर ने उनकी आवश्यकताओं का पता लगाया और उनकी तिरुपति की यात्रा की व्यवस्था कर दी। किसी प्रकार से देवकृत व्यवस्था से डिब्बे में इनके पार्श्व में बैठने वाला यात्री मलयाला स्वामी का भक्त निकला। श्रीधर का उद्देश्य सुन कर इस सज्जन ने सुबेदार षण्मुखम् नामक मलयाला स्वामी के आश्रम के एक अन्तेवासी के नाम एक परिचय-पत्र लिख दिया और इन्हें आश्वासन दिया कि इन्हें वहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। उसने सच ही कहा था; क्योंकि षण्मुखम् इन्हें मलयाला स्वामी के पास ले गये जिन्होंने इन्हें एक आश्रमवासी के रूप में वहाँ रहने की अनुमति दे दी। श्रीधर वहाँ के सादगी तथा तपस्या का जीवन-यापन करने में सुखी थे। आश्रम के अन्य सन्तों की भाँति वह मध्याह्न में उदरभर भोजन और रात्रि में केवल कुछ चना, गुड़ तथा थोड़े-से घी पर रहा करते थे। मलयाला स्वामी ने, जो तिरुवन्नामले में दीर्घकालिक तपस्या करके एक महान् तपस्वी बन चुके थे, श्रीधर पर अपना प्रभाव डाला। वह अपना जाग्रतकाल दिव्य नाम के जप, गीता के स्वाध्याय, प्रार्थना तथा मलयाला स्वामी के दर्शन में व्यतीत करते हुए कुछ सप्ताह वहाँ रहे।
इस बीच उनके सम्बन्धी तथा मित्र उनको खोज निकालने की सभी आशा त्याग चुके थे। बड़े ही चमत्कारिक ढंग से श्रीनिवास राव के सेवकों में से विश्वनाथ नामक एक सेवक को एक दिन ऐसा लगा कि वह श्रीधर का पता लगा सकता है। बिना किसी निश्चित विचार के कि वह व्यासाश्रम क्या करने जा रहा है, अपनी अन्तःप्रेरणा से वहाँ के लिए चल पड़ा और वहाँ अपने किशोर स्वामी को पा कर उसे महान् आनन्द तथा आश्चर्य हुआ। उसने श्रीधर के सम्मुख उनकी अनुपस्थिति से घर में उत्पन्न दुःख तथा चिन्ता का वर्णन किया। उसने अपना यह संकल्प अभिव्यक्त किया कि जब तक श्रीधर उसके साथ घर जाने को सहमत नहीं होते, वह अन्न-जल नहीं ग्रहण करेगा। श्रीधर को विशेषकर इस कारण झुकना पड़ा कि स्वयं मलयाला स्वामी ने उन्हें अपनी यथाविधि शिक्षा कुछ और आगे तक चालू रखने को कह कर उन्हें इसी प्रकार का परामर्श दिया था। श्रीधर को यह स्पष्ट हो गया कि उनके घर तथा परिवार का त्याग करने का नियत समय अभी तक नहीं आया है। उन्होंने बिना किसी निर्वेद अथवा निराशा की भावना के भगवदिच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने मलयाला स्वामी से केवल यह प्रार्थना की कि उन्हें कुछ और अधिक समय तक वहाँ रहने की अनुमति प्रदान की जाये जिससे वह स्वामी की, जो अभी तक श्वेत वस्त्र में थे, संन्यास-दीक्षा देख सकें। प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी। कुछ दिन पश्चात् वाराणसी के परम पावन श्री स्वामी शंकरानन्द गिरि मलयाला स्वामी को परम पावन संन्यासाश्रम में दीक्षित करने के लिए व्यासाश्रम आये। वह मलयाला स्वामी के विपुल परिजनों के साथ सम्मिलित हुए और कालहस्ती में भगवान् शिव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ गये। इस लघु तीर्थयात्रा के पश्चात् महान् गुरु शंकरानन्द गिरि व्यासाश्रम वापस आये और 'विरजा होम' नामक विशेष हवन सम्पन्न करके मलयाला स्वामी को संन्यास-दीक्षा दी। मलयाला स्वामी ने अब नया नाम असंगानन्द गिरि धारण किया। वह अपने गुरु के स्पर्श से तत्काल गम्भीर ध्यान में शब्दार्थतः निमग्न हो गये। क्योंकि वह भागवत सत्ता में दीर्घ काल तक तल्लीन रहे, अतः श्रीधर ने इस महान् सन्त को मौन रूप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पूर्व-आदेशानुसार व्यासाश्रम से प्रस्थान किया।
वह प्रतिवाद अथवा वाद-विवाद की किसी प्रकार की बड़बड़ाहट बिना वापस आ गये; क्योंकि उन्होंने अपनी गुप्त तथा गूढ़ विधि से अन्तर्ज्ञान द्वारा यह पूर्ण रूप से समझ लिया कि उन्हें नियत समय के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। परिवार के लोग इससे अत्यधिक चिन्तारहित तथा आनन्दित हुए कि एक गम्भीर संकट टल गया, किन्तु किसी की समझ में यह आया नहीं प्रतीत होता कि यह तो केवल उपक्रम के रूप में था और श्रीधर के पूर्ण त्याग का समापक कार्य एक दिन अवश्यम्भावी घटना का रूप ले कर रहेगा। वे उन्हें सभी प्रकार से शान्त करना चाहे तथा उन्होंने उनसे अपने प्रपलायन का कारण बतलाने के लिए अनुनय-विनय की। श्रीधर ने संन्यासी बनने की अपनी इच्छा प्रकट रूप से प्रथम बार ज्ञापित की जिससे कि वह दीर्घकालिक अजस्र साधना प्रारम्भ कर सकें। उनके फूफा तथा आध्यात्मिक परामर्शदाता आर. कृष्ण राव ने उन्हें लोयोला महाविद्यालय में अपना अध्ययन पूरा करने तथा अपनी उपाधि ग्रहण कर लेने के अनन्तर ही अपनी भावी कार्यविधि के विषय में निर्णय लेने का परामर्श दिया। श्रीधर अपने फूफा की इच्छाओं का सदा ही सम्मान करते थे। वह स्वाग्रह त्याग दिये जिससे उनके सम्बन्धियों ने सुख की श्वास ली। उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि श्रीधर जैसे कृतसंकल्प व्यक्तियों के किसी कार्य के स्थगन का अर्थ संकल्प का न्यूनीकरण नहीं हुआ करता।
अपनी बात के धनी, श्रीधर अब अपने अध्ययन में निमग्न हो गये और यद्यपि तैयारी के लिए अत्यल्प समय बच रहा था, फिर भी वह पाठ्य-विषय पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा बिना किसी कठिनाई के उत्तीर्ण कर ली। किन्तु अब यह परिवर्तित व्यक्ति थे। वह अहर्निश आध्यात्मिक विचारों से आप्तावित रह अपना जीवन यापन करते थे। रमण महर्षि तथा स्वामी असंगानन्द गिरि (मलयाला स्वाभी जी) के सम्पर्क ने उनके मानसिक धरातल तथा आचरण पर अमित विहाया। जब वह एक संन्यासी की तरह मुण्डित शिर तथा खादी टोपी पहने हुए तथा प्रशान्त मनोदशा में अपने महाविद्यालय में वापस गये तो इनके भों ने प्रथम यह समझा कि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु का शोक है, बना उन्हें वास्तविक कारण जानने तथा यह अनुभव करने में देर न लगी कि उसके बाद में एक असाधारण व्यक्ति है जिसकी सम्पूर्ण सत्ता अब एक रहस्यमयी विभूति की उन्मुख है।
निवृत्ति की प्रबल आन्तर धारा के होते हुए भी उन्होंने अपने शैक्षिक कार्य को चित्ररूपरता से सम्पन्न किया। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने अध्ययन के क्षेत्र को विस्तृत करने में भी किया। धर्मग्रन्थों तथा साधु पुरुषों द्वारा लिखित पुस्तकों के आयन के अतिरिक्त वह अपना पर्याप्त समय अँगरेजी-साहित्य के अध्ययन में ते थे। वह अपने मित्र श्री एन. सुब्रह्मण्यम् के साथ कभी-कभी घण्टों तक इरियर तथा अन्य अँगरेजी लेखकों पर चर्चा किया करते थे। वह पलायनवादी नहीं थे और न उन्होंने कभी अपने जीवन में पराजय ही स्वीकार की। उन्होंने अपनी है. ए. की परीक्षा अँगरेजी में सगौरव उत्तीर्ण की और सम्पूर्ण मद्रास महाप्रान्त में सन् १९३८ में पंचम स्थान प्राप्त किया।
स्नातक बनने के पश्चात् उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक साधना के लिए पर्याप्त समय ग्राम हुआ। उन्होंने न तो लौकिक जीवन-वृत्ति में और न भौतिक उन्नति में कोई उत्सुकता प्रदर्शित की। उन्होंने अपने फूफा को बी. ए. की उपाधि प्राप्त कर लेने के पाचात् हो संन्यास के विषय में सोचने का वचन दिया था। एक अन्य वचनबद्धता भी इथे। उनकी मातामही ने उनके जीवित रहने तक परिवार के सम्बन्ध का परित्याग न करने का बादा उनसे ले लिया था। श्रीधर अपने जीवन में सदा ही दूसरों का सर्वाधिक ध्यान खते थे। वह अपनी मातामही सुन्दरम्मा के लिए अपनी पुत्री सरोजिनी (श्रीधर की माता) की दुःखद क्षति की गम्भीरता से अवगत थे। वह 'मनोहर-विलास' को सदा के लिए अलविदा कह कर उन्हें अन्य प्रचण्ड आघात नहीं पहुँचाना चाहते थे। अतएव वह मातामही सुन्दरम्मा के कारण घर में रहते रहे; किन्तु वह अपने को अलग रखते थे कार जीवन-यापन करते थे। वह अपना कुछ समय किशोर फुफेरे भाइयों तथा अल्पवयस्क मित्रों को दिव्य जीवन की शिक्षा देने तथा उन्हें धर्मनिष्ठा, आर्जव, सत्यवादिता तथा साथियों की सेवा में अवगुण्ठित सूक्ष्म तत्त्वों को समझाने में लगाते। एक ऐसे ही अल्पवयस्क साधक श्री वेंकोबा श्रीधर से अत्यधिक प्रभावित थे। श्रीधर के सरल तथा सन्तसुलभ जीवन का उन पर ऐसा शक्तिशाली प्रभाव पड़ा कि उन्होंने श्रीधर से मन्त्रदीक्षा देने की प्रार्थना की। श्रीधर ने उन्हें निराश नहीं किया। यद्यपि वह संन्यासी नहीं थे, फिर भी उन्होंने न तो कातरता और न संकोचशीलता अनुभव की। वह जानते थे कि वह राम में रह रहे हैं और यही पर्याप्त था। तेईस वर्षीय गम्भीर तथा आत्मविश्वासपूर्ण इस नवयुवक ने श्री वेंकोबा को महान् राम तारकमन्त्र की दीक्षा दी। और उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि ऐसी थी कि दीक्षा ने किशोर फुफेरे भाई में तत्काल और दूरगामी परिवर्तन लाया।
यह स्मरणीय है कि इन सभी आध्यात्मिक तल्लीनताओं में भी उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों तथा साथियों के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की। द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने के कारण चेन्नै नगर संकट के प्रभाव में आ गया था। शासकीय संस्तुति से चेन्नै नगर की जनता का व्यापक निष्कमण हो रहा था। सम्पूर्ण 'किम्बर्ली' परिवार चेन्नै छोड़ कर कोयम्बतूर आ बसा और किम्बर्ली कोठी अस्थायी रूप से भाड़े पर दे दी। इस समय श्रीधर अपने ताऊ जी. कृष्ण राव के दिन-प्रति-दिन के घरेलू कार्यों में विशेष रूप से तथा कुछ मात्रा में जागीर के काम में भी सहायक थे। रोचक बात तो यह है कि श्रीधर के पिता ने उनसे किसी प्रकार का कार्य कराने में कभी भी रुचि प्रदर्शित नहीं की। वह जानते थे कि श्रीधर सत्त्वहीन नीरस पारिवारिक दायित्वों के लिए नहीं हैं। उनकी सहजानुभूत धारणा थी कि उनका पुत्र उन लोगों में से नहीं है वरन् वह तो उन्मुक्त गगन की मुक्त आत्मा है; अत: उसे पारिवारिक धन्ों तथा दायित्वों में बाँधने का प्रयास करना निरर्थक ही होगा। वह जानते थे कि श्रीधर भगवान् की महिमा की घोषणा करने के लिए विस्तीर्ण जगत् में भाग जाने को अपने को पक्षी की भाँति स्वतन्त्र रखेंगे। अतएव उनके पिता श्रीनिवास राव ने युवक साधक को कभी भी किसी प्रकार के पारिवारिक दायित्व अथवा सामाजिक कर्तव्यों से निरुद्ध अनुभव नहीं होने दिया। परन्तु श्रीधर ने स्वेच्छा से ही परिवार की विविध रूपों से सेवा की। उनकी आध्यात्मिकता स्वार्थपरायण प्रकार की नहीं थी जो लोगों को अपने सम्बन्धियों की आवश्यकताओं तथा प्रत्याशाओं के प्रति अस्वाभाविक और अंसवेदनशील रूप से निष्ठुर बना देती है। उदाहरणार्थ, इसी अवधि में इनके बहनोई डा. बी. एन. के. शर्मा किसी गम्भीर रोग से दीर्घकाल तक शय्याग्रस्त रहे। उस समय इन्होंने मातृ-सुलभ स्नेहिल चिन्ता से सेवा-सुश्रूषा कर उन्हें पुनः स्वस्थ किया; किन्तु अपने परिवार के सदस्यों के प्रति ऐसी सभी सहानुभूतियों तथा सेवाओं के मध्य भी उन्होंने कभी भी अपने को आसक्ति की अवस्था में पड़ने नहीं दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया, उसमें वह सर्वथा निस्स्वार्थ तथा मिथ्याभिमान-रहित, अतएव नितान्त अदूषित बने रहे। इस प्रकार वह अथक साधना में आगे बढ़ते रहे। वह अपने चित्त को उलझाये बिना परिवार की शारीरिक सेवा करने के लिए अपने को पर्याप्त परिपक्व अनुभव करते थे तथा सभी बन्धनों को तोड़ कर मुक्त होने और अन्ततः संन्यास-जीवन ग्रहण करने के उपयुक्त अवसर की मन ही मन प्रतीक्षा में थे।
वह सन् १९४० में कांजनगढ़ के स्वामी रामदास (पापा) से चेन्नै में मिले। उनकी प्रिय मातामही सुन्दरम्मा का निधन उसी वर्ष हुआ। उन्होंने लौकिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के द्वारा उपाधि प्राप्त कर ली थी और उसके द्वारा अपने फूफा आर. कृष्ण राव तथा अपनी मातामही को दिये हुए अपने वचन को पूरा कर लिया था। उन्होंने स्वेच्छा से अपने को लोक-लिहाज के जिस बन्धन के अधीन किया था, वह अब निरस्त हो गया और श्रीधर अन्य किसी वचनबद्धता से अपने को आबद्ध नहीं किये थे। इस समय स्वामी रामदास के साथ उनके मिलन का अवश्यम्भावी प्रभाव पड़ा। सन् १९२८ में ही इन्होंने स्वामी रामदास के विषय में सुना और तभी से वह इनके महान् प्रेरणा-स्रोत बने रहे। रामदास की प्रथम बार जानकारी प्राप्त करने की एक रोचक कथा है। उनके बाल्यकाल में अनेक अधिकारी तथा सज्जन एन. वेंकट राव के साथ टेनिस खेलने के लिए 'मनोहर-विलास' आया करते थे। स्थानीय नगरपालिका के एक निरीक्षक नियमित अभ्यागत थे। वह कभी-कभी अपने अनुज के विषय में चर्चा किया करते थे जो संन्यासी का जीवन-यापन करने के लिए अपने सांसारिक जीवन को तिलांजलि दे चुके थे। उस निरीक्षक का अनुज अन्य कोई नहीं, श्रीधर के प्रिय 'पापा' स्वामी रामदास थे। इस भाँति इस मिलन से दिव्य भावातिरेक का प्रबल ज्वार-भाटा उमड़ पड़ा। सन्त को भी नवयुवक में ज्वलन्त कामना देख कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। रामदास ने भगवान् राम की कृपा का आह्वान कर उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रीधर को अब सन्त की आत्मकथा के शब्द स्मरण हो आये : "रामदास! त्याग के उन्नत शिखर पर आरूढ़ हो जाओ और वहाँ से अपने चतुर्दिक् के सम्पूर्ण दृश्य-प्रपंच के अनित्य स्वरूप का अवलोकन करो। प्रत्येक स्थान पर तुम जन्म, वार्द्धक्य तथा मृत्यु ही देखोगे। सभी विनाश के एक ही पथ पर भागे जा रहे हैं।" रामदास ने श्रीधर की पहले से ही उव बनी हुई मन-भूमि को अपने आशीर्वाद की वृष्टि से आप्लावित कर दिया। बीज के प्रस्फुटित होने के लिए यही पर्याप्त था।
रामदास के साथ इस मिलन के तुरन्त बाद ही भगवान् ने नवयुवक को एक लुभावना प्रस्ताव भेजा मानो कि वह उनके मन की परीक्षा लेने के लिए हो। वह राजकीय वायु-सेवा में बहुत ही मोहक सम्भावनाओं से युक्त विमान चालक के पद के लिए चुन लिये गये। उन दिनों परिवार अपेक्षाकृत आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। अतः प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना श्रीधर के लिए सभी दृष्टियों से एक अभिनन्दनीय निर्णय होता; किन्तु वह तो पहले से ही एक ऐसे मार्ग पर प्रस्थान कर चुके थे जो उन्हें ऐसी ऊँचाइयों पर ले जाने वाला था जहाँ कोई भी वायुयान कभी भी आरोहण नहीं कर सकता। इससे इनमें प्रलोभन की क्षणिक स्फुरणा भी नहीं उत्पन्न हुई। तथापि उन्हें अपनी अस्वीकृति के कुछ कारण प्रस्तुत करने थे। अतएव प्रशिक्षण के चयन-पत्र की प्राप्ति की सूचना देते तथा उसके लिए अपना आभार प्रकट करते हुए उन्होंने शिश्तापूर्वक निवेदन किया कि चूँकि वह आमिष भोजन नहीं लेते और चूँकि इससे विचारणीय कार्य के सामाजिक वातावरण में भद्दी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः वह प्रस्ताव को अस्वीकार करना अधिक पसन्द करते हैं। भला वह महान आत्मा जिसने असंख्य सच्चे पिपासुओं को उनकी मुक्ति की यात्रा में उनके जीवन-पोत का पथ-प्रदर्शन करने के लिए जन्म लिया हो, एक वायु-सेना के यान-चालक के आडम्बरपूर्ण व्यक्तित्व में क्योंकर सिमट सकती थी।
प्रस्ताव को शिष्टतापूर्वक अस्वीकार करने के उपरान्त श्रीधर अब संन्यास-ग्रहण करने के लिए कृतसंकल्प थे। वह अपनी परीक्षा कठोरतापूर्वक ले चुके थे और मठवासी जीवन के लिए तैयार हो चुके थे। उनका वैराग्य विचार पर आधारित तथा दीर्घकालीन ध्यान तथा आत्म-निरीक्षण से पोषित था। अतः स्वामी कृष्णानन्द के शब्दों में "अब भारत की आत्मा के अन्तरतम रहस्य ने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया।" किन्तु इस क्षण भी श्रीधर में दूसरों के प्रति चिन्ता अनुकरणीय थी। उन्होंने अपनी अनुजाओं-वसुधा तथा वत्सला-और छोटी मौसी मालती बाई को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने संन्यास-ग्रहण की इच्छा सूचित की। वत्सला उस समय केवल सोलह वर्ष की बालिका थीं। श्रीधर ने हृदयस्पर्शी शब्दों में उनसे कहा कि उन सबकी तथा विशेषकर वत्सला की देखभाल करना उनका दायित्व है; किन्तु भगवान् के लिए उनकी उत्कण्ठा ने सांसारिक वातावरण में उन्हें दुःखी बना दिया है। उन्होंने अपनी आश्रित बहनों तथा मौसी में से प्रत्येक से बड़ी ही गम्भीरतापूर्वक पूछा कि वे सच्चाई से उन्हें बतायें कि क्या वे बिना किसी पश्चात्ताप तथा शोक के उन्हें चले जाने की अनुमति देंगी। उन्हें मालूम था कि भगवान् उनकी ऐसी देख-रेख करेंगे जैसा कोई भाई अथवा भतीजा नहीं कर सकेगा। किन्तु निर्णय उन्हें करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनमें से एक की भी ऐसी इच्छा हुई तो वे सब जब तक अन्तिम रूप से जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हो जार्ती तब तक वह घर पर ही बने रहेंगे। एक सिद्ध माया के साथ खिलवाड़ कर रहा था। माया अत्यधिक बलवती है; किन्तु राम के सेवक के समक्ष वह विवश है। श्रीधर की अभ्यर्थना इतनी गम्भीर थी और ये अभिनव वयस्क लोग आध्यात्मिक संस्कारों से इतने पूर्ण थे कि उनमें से प्रत्येक ने उन्हें चले जाने के लिए पूर्ण तथा मुक्त अनुमति दे दी। उन्होंने दृढ़ विश्वास तथा गम्भीर भाव से अनुभव किया कि जो भगवान् अजगरों को भोजन तथा आकाशचारी निस्सहाय पक्षियों को दैनिक आहार प्रदान करता है, वह वही भगवान् है जिसने उन्हें लौकिक जीवन को त्याग करने को अभी प्रेरित किया। उन्होंने अनुभव किया कि वही भगवान् उनकी आवश्यकता के समय निश्चय ही अपना त्राणदायक हाथ उन सबकी ओर बढ़ायेगा तथा उनकी सँभाल करेगा। भारतवर्ष के दिव्य परिवारों की जय हो जो ऐसे उदात्त भावों तथा उत्कृष्ट आदर्शों को सम्पोषित करते हैं।
श्रीधर का मार्ग अब निर्बाध था। वह ऋषिकेश के स्वामी शिवानन्द के साथ पहले ही से सम्पर्क में थे और उनसे निवृत्ति-मार्ग पर चलने के लिए निर्भयतापूर्वक आगे बढ़ने का परामर्श प्राप्त हो चुका था। उन्होंने अब देखा कि उन्मुक्त स्वतन्त्रता का आनन्दपूर्ण दिवस आने ही वाला है। तथापि उन्होंने निर्णायक छलाँग लगाने से पूर्व चार सन्तों को उनके आशीर्वाद के लिए चार पत्र लिखे। उन्होंने उल्लेख किया कि वह जन्मजात ब्राह्मण हैं तथा गृह तथा परिवार का त्याग करने तथा निवृत्ति-मार्ग पर चलने का महत्त्वपूर्ण पग उठाना चाहते हैं तथा इसके लिए उनके आशीर्वाद की याचना की। उन्होंने रमण महर्षि, स्वामी रामदास, स्वामी राजेश्वरानन्द तथा रामकृष्ण मिशन के स्वामी अशेषानन्द को एक ही शैली में पत्र लिखे। उन सभी लोगों ने श्रीधर को अपने आशीर्वाद प्रेषित किये और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। श्रीधर ने शिरडी के साई बाबा के आश्रम के व्यवस्थापक को भी पत्र लिखा। उन्हें बाबा के आशीर्वाद के प्रतीक-रूप में उनका प्रसाद प्राप्त हुआ।
अब तो एक क्षण भी नष्ट करने को नहीं था। "न कर्मणा न प्रजया धरन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः न तो कर्म से, न सन्तान से और न ही धन से करन एकमात्र त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है।" महानारायणोपनिषद् (१२-१४) के दे शब्द उनके कानों में गूँज रहे थे। हृद५ में अनिर्वचनीय आनन्द लिये हुए, गम्भीर मन से श्रीधर ने ६ मार्च १९४३ को कोयम्बतूर के अपने गृह से बहिर्गमन किया। वह एक महत्त्वपूर्ण दिवस था जब उन्होंने जिस सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन में सत्ताईस वर्ष पूर्व वह उत्पन्न हुए थे, उसे अन्तिम रूप से त्याग दिया। उनके पिता तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों के लिए अवश्यम्भावी घट चुका था और वे उसे स्वीकार कर चुके थे। अन्ततः श्रीधर श्वेत वस्त्र में सदा संन्यासी ही तो थे। उनके लिए त्याग तो मात्र एक औपचारिक कार्य था। स्वामी वेंकटेशानन्द ने ठीक ही कहा है: "उनको अपने लिए ऐसा कोई प्राप्तव्य पदार्थ न था जो उन्हें पहले से ही प्राप्त न हो। उन्हें कभी भी किसी वस्तु से आसक्ति न थी जिसे उन्हें त्याग करना हो। वह कभी गृहस्थी नहीं थे जिससे उन्हें संन्यास लेना हो। वह कभी भी सांसारिक व्यक्ति नहीं थे जिससे उन्हें संसार का त्याग करना हो। वह जन्म से ही यह सब-कुछ थे-सबसे अनासक्त एक योगी, एक उत्कृष्ट कोटि के संन्यासी, एक महान् सन्त तथा इन सबसे अधिक।" अतः जन्मजात सिद्ध ने अब लोक-संग्रह के लिए गृह-त्याग किया।
कोयम्बतूर से वह भगवान् वेंकटेश्वर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तिरुपति की ओर अग्रसर हुए। यहाँ वह कुछ समय तक रहे तथा अपने अहं को मिटाने के लिए अपने को परीक्षा तथा अनुशासन में डाला। उन्होंने एक ठेकेदार से दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर उन्हें शारीरिक श्रम का कोई कार्य देने के लिए निवेदन किया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से एक लब्धप्रतिष्ठ ब्राह्मण-परिवार तथा लब्धप्रतिष्ठ शैक्षिक जीवन के मनोवैज्ञानिक अवशेष को-यदि अब भी कुछ अवशेष था-हटाने के लिए वहाँ एक श्रमिक के रूप में कार्य किया। उन्होंने निर्माण-स्थल पर विनम्रतापूर्वक कठोर श्रम किया। उन्होंने कुछ दिनों तक पूर्ण सच्चाई से कार्य किया और तब अपने नियोजक से जाने की अनुमति माँगी। ठेकेदार ने उन्हें उनका पारिश्रमिक दिया, किन्तु उन्होंने प्रेम तथा कृतज्ञता के प्रतीक-रूप में केवल एक रुपया लिया और नम्रता के पोषण के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करने के लिए भगवान् के प्रति अपनी कृतज्ञता के रूप में भगवान् वेंकटेश्वर के चरणों में कुछ पुष्पों के साथ वह रुपया अर्पित करने चले गये। स्वामी शिवानन्द ने भी अपनी संन्यास-दीक्षा से पूर्व घालज के डाकपाल के अधीन रसोइये का कार्य करके इसी प्रकार के अनुशासन को झेले थे। इस विषय में शिवानन्द तथा चिदानन्द एक ही साँचे में ढले थे।
श्रीधर ने तिरुपति से महान् साई बाबा के समाधि-स्थान शिरडी की यात्रा की। शिरडी नासिक के समीप एक छोटा-सा ग्राम है। यहाँ श्रीधर १९४३ के पचित्र रामनवमी-दिवस, २० अप्रैल तक पूरे एक मास तक रुके। वहाँ उन्होंने रामनवमी के अवसर पर महोत्सव देखा जिसमें अगणित भक्तजन साई बाबा की पवित्र समाधि का अभिषेक करने के लिए पन्दरह मील दूर से गोदावरी नदी से पवित्र चल ले कर आये। यहाँ श्रीधर सहस्रबुद्धे नामक एक आरक्षी अधिकारी से मिले जो साई बाबा के सम्पर्क से एक आध्यात्मिक व्यक्ति में बदल गया था और सामान्यतया दास गनु महाराज के नाम से विख्यात था। साई बाबा के आश्रम के अपने आवास काल में वह स्वेच्छा से कठोर श्रम करते, पुस्तकालय-महाकक्ष की सफाई करते तथा अन्य प्रकार की स्वैच्छिक सेवाएँ अर्पित करते थे। व्यवस्थापकगण चाहते थे कि श्रीधर वहाँ के स्थायी आवासी बन जायें; किन्तु वह अपने गुरु की खोज में अब एक परिव्राजक थे। अतः रामनवमी के पश्चात् वे शिरडी से प्रस्थान कर भगवान् कृष्ण के नित्य लीला-स्थल वृन्दावन की ओर चल पड़े। यहाँ उन्होंने वृन्दावन के वंशीधर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा स्थानीय रामकृष्ण मठ में पन्दरह दिन रुके। वृन्दावन से उन्होंने स्वामी शिवानन्द जी महाराज को एक पत्र लिख कर सूचित किया कि वह अपना घर तथा परिवार त्याग चुके हैं और एकान्त में साधना के लिए स्थायी रूप से रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान की खोज में चल पड़े हैं। स्वामी जी ने उत्तर में लिखा कि वह अभी तरुण ही हैं; अत: अभी उन्हें अपने सम्बन्धियों की सेवा करते रहनी चाहिए, अध्यापन-कार्य करना चाहिए तथा रोगियों की सेवा करनी चाहिए। इस उत्तर से उन्हें महान् आश्चर्य हुआ और इस परामर्श से आश्चर्य इस कारण हुआ कि स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने अपने पूर्वगामी पत्रों में उन्हें तत्काल संसार त्याग करने के लिए बार-बार उपदेश दिया था। यह वस्तुतः श्रीधर की अन्तिम परीक्षा थी। माया के अनेक रूप हो सकते हैं। उच्च कोटि के लोगों के लिए माया प्रतीयमानतः अविजेय मानव-आदर्शों का सूक्ष्म रूप धारण करती है। गुरुदेव स्वामी शिवानन्द श्रीधर के संसार से वैराग्य तथा भगवान् में अनुराग की गहराई की केवल परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे थे। श्रीधर के उत्तर से यह स्पष्ट हो गया कि वह माया से परे जा चुके हैं। उन्होंने गुरुदेव को केवल यह सूचित करने को एक संक्षिम पत्र लिखा कि अब घर प्रत्यावर्तन की बात उनके लिए अव्यवहरणीय है तथा उन्होंने पहले से ही उनके चरण-कमलों में शरण लेने का निर्णय कर लिया है। गुरुदेव इस पत्र से अत्यधिक सन्तुष्ट हुए तथा अपना स्वीकृति-सूचक पत्र भेज दिया।
श्रीधर ने वृन्दावन से अपने निर्णायक तथा दृढ़ निश्चय के विषय में गुरुदेव को अपना अन्तिम विचार लिख भेजा। तत्पश्चात् उन्होंने हरिद्वार की यात्रा की जहाँ वह कनखल में रामकृष्ण मिशन में दश दिन तक रुके। अब वह अपने गुरुदेव से मिलने तथा सदा-सर्वदा के लिए उनके चरण-कमलों में आत्मसमर्पण करने को उत्सुक थे। उनकी भावनाओं ने सन् १९४३ के बुद्ध-पूर्णिमा-दिवस को दृढ़ संकल्प के रूप में निश्चित आकार ले लिया। १९ मई का अतीव उष्ण दिवस था जब अपराह्न के २ बजे उन्होंने बस द्वारा ऋषिकेश को प्रस्थान किया। यह दिवस श्रीधर के जीवन में, दिव्य जीवन संघ के इतिहास में तथा बीसवीं शती के आध्यात्मिक नवचेतना के इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। सादे मोटे खद्दर का कुरता तथा पायजामा पहने तथा हाथ में एक लाठी लिये हुए श्रीधर ने शिवानन्दाश्रम में सादगी से प्रवेश किया। उस समय सायंकाल के लगभग पाँच बजे थे। स्वामी शिवानन्द जी ऊपर पहाड़ी पर भगवान् विश्वनाथ के मन्दिर में गये हुए थे। एक नेपाली भारवाहक ने श्रीधर को स्वामी शिवानन्द के पवित्र आश्रम के निकटवर्ती रामाश्रम-पुस्तकालय के निकट प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया। वहाँ श्रीधर अपने हाथों में मिश्री तथा गम्भीरतम भक्ति से सिक्त नेत्रों के साथ प्रतीक्षा करने लगे। सन्ध्या सघन होती जा रही थी। पवित्र बुद्धपूर्णिमा का पूर्णेन्दु अभी-अभी उदित हुआ था। गुरुदेव मन्दिर से लम्बे डग भरते हुए पहाड़ी से नीचे आये। जब गंगा शान्तिप्रद चन्द्रिका में झिलमिला रही थी, दिव्य जीवन संघ के भावी पूर्णेन्दु ने आनन्द-कुटीर की ज्ञान-ज्योति को प्रणाम किया। श्रीधर ने अपने आध्यात्मिक पिता का दर्शन किया। उन्होंने अपने मधुर तथा विनम्र आत्मसमर्पण के प्रतीक-रूप में मिश्री अर्पित करते हुए गुरुदेव के चरण-कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। भूमि पर तीन बार साष्टांग प्रणाम करने के अनन्तर उन्होंने अत्यधिक विनम्रतापूर्वक सूचित किया कि वह चेन्नै के श्रीधर राव हैं। गुरुदेव ने उनसे एक मराठी वाक्य में उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछा मानो वह उनसे चिरकाल से परिचित हों। उनके लिए श्रीधर किंचित् भी अपरिचित नहीं थे। वह जानते थे कि उनका उत्तराधिकारी आ गया है। श्रीधर को भी इस प्रकार का अनुभव हुआ। उनके लिए यह रुचिकर गृहप्रत्यागमन-सा था। गुरुदेव ने बड़े ही अनौपचारिक ढंग से उन्हें सायंकालीन सत्संग में उपस्थित होने तथा आगामी दिवस के बड़े प्रातः ही अपने कुटीर में उनसे मिलने के लिए कहा।
इस भाँति अन्त में श्रीधर को शिवानन्द के चरण-कमलों में अपना स्थिरक प्राप्त हो गया । गुरु भगवान् हैं। भगवान् गुरु हैं। भगवान् श्रीमद्भागवत में कहते हैं: "वास्तव में आचार्य को मुझे (भगवान्) ही जानो। उनकी कभी भी अवज्ञा न करो और न उनको केवल मानव मान कर कम महत्त्व दो। गुरु में सभी देव सम्पुटीकृत हैं।" अब श्रीधर अपने परम देव के, अपने गुरु के, जगद्गुरु स्वामी शिवानन्द के, भगवत्साक्षात्कार- प्राप्त एक महान् आत्मा के सन्मुख थे। उन्होंने भगवान् की खोज में सुदूर स्थानों की यात्राएँ की थीं और अब वह प्रतिज्ञात देश के प्रवेश-द्वार पर पहुँच गये।
तृतीय अध्याय
शिष्यत्व के बीस वर्ष
"योगः कर्मसु कौशलम्
-कर्म करने का कौशल ही योग है" (गीता : २-५०)।
श्रीधर ने ऋषिकेश की पावन भूमि में उस भाग्य-निर्णायक दिवस को अपने को जिस असाधारण आध्यात्मिक गुणों से सम्पन्न व्यक्ति की देख-रेख में अर्पित किया, उसका जन्म मद्रास के तिरुनेल्वेलि जिले के पत्तमडै ग्राम में ८ सितम्बर १८८७ को हुआ था। वह यशस्वी सन्त प्रख्यात शैव आचार्य अप्पय दीक्षित की अठारहवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे। कुप्पुस्वामि, जैसा कि वह उन दिनों कहलाते थे, अपनी धर्मपरायणता के लिए प्रख्यात दम्पति वेंगु अय्यर तथा पार्वती अम्माल की गोद में उत्पन्न हुए थे। कालक्रम से विकास पा कर वह एक प्रतिभाशाली युवक बने। निर्धनों तथा रोगियों की ओर स्वभावतः आकृष्ट होने के कारण वह चिकित्सीय शिक्षा प्राप्त करने गये तथा एक डाक्टर की उपाधि प्राप्त की। दैवयोग से वह मलया गये जहाँ उन्होंने लगभग एक दशक तक लोगों की सेवा की। भारत का यह नवयुवक डाक्टर निर्धन तथा धनवान्, परिष्कृत तथा निरक्षर सभी से समान रूप से परिचित था। इसने एक भद्र समारी (दानशील) के रूप में शीघ्र ख्याति अर्जित कर ली। उनके लिए कर्म भगवदुपासना था। यद्यपि अपने सजातीयों का दुःख उन्हें निरन्तर क्रियाशील बनाये रखता तथापि उनका प्रारम्भ का उफान शनैः -शनैः शान्त हो चला और उनमें एक विचारशील, चिन्तनशील प्रकृति का विकास हुआ। वह धार्मिक साहित्य का बहुत अधिक परिशीलन करने लगे। धीरे-धीरे उनमें यह सत्य प्रकट हुआ कि रोगों, पीड़ाओं, मानसिक व्यथाओं तथा अश्रुओं से युक्त इस संसार से परे निःश्रेयस, आनन्द तथा चिरन्तन शान्ति की अवस्था है और यह एक ऐसी वस्तु है जिसे प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव एक समृद्ध जीवन-वृत्ति को तिलांजलि दे सन् १९२३ में वह एक दिन चुपचाप मलया से चल पड़े और एक पथप्रदर्शक तथा तप करने के लिए उपयुक्त वातावरण की खोज में हिमालय आ गये। वह ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर स्वामी विश्वानन्द से मिले तथा उनसे पवित्र दीक्षा देने की याचना की। इस भाँति वह १ जून १९२४ को पवित्र संन्यास-आश्रम में दीक्षित हुए। स्वामी शिवानन्द के नाम से विश्रुत अब वह सन् १९२४ में ऋषिकेश में स्थायी रूप से रहने लगे। उन्होंने लगभग एक दशक तक कठोर तपस्या, योगाभ्यास तथा गहन ध्यान का अभ्यास किया तथा भगवान् के आशीर्वाद से आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर एक जीवन्मुक्त के रूप में वह विभासित हुए ।

गुरुदेव का चरण अनुसरण करते हुए

परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में
हिमालय के इस अद्वितीय सन्त के लिए गुरुपन एक विनाशकारी रोग था; किन्तु सर्वशक्तिमान् प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसने अपना ध्यान लोक-संग्रह की दिशा में मोड़ा। उसने सन् १९३६ में दिव्य जीवन संघ की स्थापना की तथा भारत के कोने-कोने तक बल्कि समूचे भूमण्डल में योग तथा वेदान्त के सन्देश का प्रचार किया। बह मानव की सेवा करने तथा उसे मोहनिद्रा से उद्बुद्ध करने के लिए जीवन-यापन करते थे। सेवा, प्रेम, दान, पवित्रता, ध्यान, आत्मसाक्षात्कार-ये उनकी उपदेश-माला के आधार थे। प्रकाशित साहित्य, व्यापक आध्यात्मिक यात्राओं, आध्यात्मिक सम्मेलनों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार तथा अन्तिम किन्तु गौण नहीं दिव्य भगवन्नाम संकीर्तन के प्रचार उनके मिशन की आधारशिलाएँ बने। संन्यासी तथा सांसारिक दोनों ही समान रूप से सहस्रों की संख्या में उनके पास एकत्र होने लगे। उन्नत साधक तथा ज्ञानवृद्ध योगी उनसे योग तथा वेदान्त का पाठ सीखने लगे और उनमें से कुछ तो आश्रमवासी के रूप में वहीं रहने लग गये। वे सभी बहुत ही सच्चे साधक थे। उनमें से कुछ बहुत ही उन्नत आत्माएँ थीं। उन्होंने अब गुरुदेव के प्रेम तथा उदारता के पवित्र उद्देश्य के सम्पादन के एक उपकरण के रूप में अपने को समर्पित कर दिया। किन्तु आनन्द-कुटीर का यह सन्त अब भी एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में था जो उसे सभी दुर्वह उत्तरदायित्वों के भार से मुक्त कर सके। वह अपने उस चुने हुए पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे वह भगवान् के शिशुओं की सेवा के लिए अपनी आध्यात्मिक निधि हस्तान्तरित कर सके। निर्दोष शुचिता तथा अपराजेय दुःसाहस वाले वह व्यक्ति थे श्रीधर, एक जन्मजात सन्त। वह उसी साँचे में ढले थे जिसमें उनके गुरुदेव। वह निर्धनों, रोगियों तथा पददलितों की सेवा में सर्वातिशायी थे। उनकी उदार आस्तिक्य बुद्धि तथा सभी प्राणियों के लिए संवेदनशील चिन्ता भी अनुपम थी। उनकी अनात्मशंसा तथा दूसरों के लिहाज का भाव दूसरों के लिए अनुकरणीय था। भक्ति तथा ध्यान की साधना उनके लिए एक स्वाभाविक, रुचिर वस्तु थी; मोक्ष की स्वतः प्रसूत ज्वलन्त कामना की परिणाम थी। उन्होंने संन्यासी की मनोवृत्ति तथा प्रकृति को ऐसे अपनाया जैसे मत्स्य जल को अपनाता है। रमण, असंगानन्द तथा रामदास जैसे सन्तों के साथ उनका सम्पर्क उनमें दिव्य चेतना की उन्नतावस्था के रूप में पहले से ही फलप्रद होने लगा था। अब वह शिवानन्द-ज्ञान की मूल्यवान् कणिकाओं को स्वाति नक्षत्र से प्रभावित शुक्तिका की भाँति अपने हृदय के अन्तर्तम प्रकोष्ठ में सँजोये हुए थे।
एक दिन गुरुदेव ने श्रीधर को अपने पार्श्व में बुलाया और कहा, "मैं यह जान कर दुःखित होता हूँ कि जब मैं अपने छात्रों पर निस्स्वार्थ सेवा हेतु अपने जीवन को ही अर्पित कर देने पर जोर देता हूँ तो वे अनेक बार मेरे भावों को समझने में असफल रह जाते हैं। मेरा यह अर्थ कदापि नहीं होता कि अपने अन्य कर्तव्यों के नाम में वे अपनी वैयक्तिक साधना की अवहेलना करें। प्रतिदिन प्रातःकाल तथा गोधूलि के समय निश्चित समय पर सुव्यवस्थित साधना शेष दिन के सक्रिय कार्य की किसी भी तरह विरोधी नहीं है। मैं जिस बात पर बल देता हूँ, वह यह है कि अकर्ता, अभोक्ता अथवा ईश्वरार्पण और निमित्तमात्र अहं भाव के अंगीकरण से कार्य भी आध्यात्मिक साधना बन जाना चाहिए।" श्रीधर ने इन ज्ञानमय शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना और तत्क्षण शिवानन्द मिशन में प्रवेश ले लिया और इस उदात्त कार्य के लिए अपनी सम्पूर्ण सत्ता समर्पित कर दी। आध्यात्मिक देवत्व उनके विचार की प्रकृति में प्रवेश कर गया और वह गुरुदेव के परम सन्तोषप्रद रूप में सक्रिय सेवा में कूद पड़े।
प्रारम्भिक प्रशिक्षण
शिवानन्दाश्रम उन प्रारम्भिक दिनों में वस्तुतः एक उटज ही था। उसके अधिष्ठाता सर्वोत्कृष्ट कोटि के एक प्रबुद्ध योगी थे। वह अपने साथ केवल आठ शिष्य रखते थे-स्वामी कृष्णानन्द जी, स्वामी विशुद्धानन्द जी, विश्वेश्वर स्वामी जी, गोविन्द स्वामी जी, पूर्णबोध स्वामी जी, शाश्वत स्वामी जी, रामचन्द्र स्वामी जी तथा नारायण स्वामी जी। ये सभी बहुत उच्च कोटि के साधक थे। नवाँ रत्न, जिसे आगे चल कर चूड़ामणि बनना था, वह थे श्रीधर राव जो शीघ्र ही राव स्वामी जी के नाम से प्रख्यात हो गये। इस नये स्वामी के लिए कोई भी कार्य निकृष्ट न था। सभी कार्य गुरुदेव के पवित्र चरणों में समान रूप से समर्पित भगवदाराधना था। स्वामी कृष्णानन्द जी ने, जो सन् १९४२ से १९४४ तक दिव्य जीवन संघ के महासचिव थे, इन्हें प्रथम पता लिखने तथा विभिन्न स्थानों को भेजने के लिए मासिक पत्रिका 'डिवाइन लाइफ' के उत्क्षेप पर नामपत्र चिपकाने का कार्य सौंपा। राव स्वामी जी परम सच्चाई के साथ पते लिखते थे। तत्पश्चात् उन्हें पुस्तकालय की पुस्तकों को व्यवस्थित करने को कहा राया। राव जी ने न केवल पुस्तकों की धूल झाड़ी और उन्हें सुरुचिपूर्ण तथा व्यवस्थित ढंग से खानों में रखा अपितु उन्होंने उन्हें आवरण से ढक भी दिया। इस कार्य में उन्होंने बही उत्साह तथा निष्कपटता दिखायी जैसे कि वह योग-साधना के लिए दिखलाते थे। बह फर्श पर झाडू लगाने, अतिथियों तथा रोगियों की देखभाल करने, टंकी को गंगा से जल ला कर भरने, फर्श पर दरी बिछाने, जंगल से ईंधन लाने, बरतन साफ करने तथा भोजनालय में काम करने, मन्दिर में पूजा करने में सहभागी बनते तथा पत्र लिखते, पाण्डुलिपि टंकिट करते तथा सायंकालीन तथा विशेष धार्मिक पर्वो पर आयोजित सत्संगों में उन्नयनकारी प्रवचन करते थे। इन सब कार्यों को करते हुए वह सदा शान्त तथा आध्यात्मिक स्फूर्ति से पूर्ण रहते थे; क्योंकि कार्य ही पूजा करने की उनकी एक प्रणाली थी। गुरुदेव एक कठोर अधिकारी, एक स्नेही पिता, एक चिन्तातुर माता तथा इनके अतिरिक्त अन्य और कुछ भी थे। उनके संस्कृत संकल्प से प्रवाहित होने वाली दिव्य कृपा तथा सदयता राव स्वामी जी को अनिर्वचनीय आनन्द से आपूरित कर देती। गुरुदेव ने शीघ्र ही अनुभव किया कि श्रीधर सामान्य व्यक्ति नहीं हैं जो किसी प्रकार के कार्य से अभिभूत हों अथवा बन्धन में आयें। उनकी उत्कृष्टतर नियति को जान कर गुरुदेव समय-समय पर उन्हें कुछ दिनों के लिए सम्पूर्ण कार्य बन्द कर एकान्त में समय व्यतीत करने को कहा करते थे। श्रीधर तत्काल चुपचाप अन्तर्मुखी अन्तरावलोकन के जीवन में चले जाते, वनों में इधर-उधर विचरण करते, एकान्त स्थानों की नीरवता तथा शान्ति पान करते तथा विश्व के स्वर से समस्वरित होने का प्रयास करते थे। जैसी और जब चाहें, वह सेवा अथवा साधना में निमज्जित होने को स्वतन्त्र थे।
रोगग्रस्तों की सेवा
शिवानन्दाश्रम में प्रवेश करने के दश दिन के भीतर ही स्थानीय जनता श्रीधर को डा. राव जी के नाम से पुकारने लगी। निश्चय ही वह उपाधिधारी चिकित्सक नहीं थे; किन्तु कुष्ठियों तथा निर्धनों की चिरकालीन तथा समर्पित सेवा से ऐसा कार्य उनका अवर स्वभाव बन गया था और वह रोगियों की परिचर्या में बहुत ही कुशल हो गये थे। यदि उनके हृदय में संसार से सम्बन्धित कोई अनुराग था तो वह यही था। उन्हें डाक्टर की पदवी ईश्वरादिष्ट परिस्थितियों में प्राप्त हुई। एक बार जब वह भ्रमणार्थ बाहर गये तो मार्ग में उन्हें एक कुष्ठरोगी मिला। उन्होंने उसे उपचार के लिए आश्रम के औषधालय में आने के लिए कहा। जब वह रोगी आश्रम में पहुँचा तो वहाँ उपस्थित प्रायः सभी लोगों ने अपनी खीज व्यक्त की। किन्तु गुरुदेव ने डा. राव को न केवल उसका उपचार करने की अनुमति दे दी, अपितु नवयुवक ब्रह्मचारी के दयामय कार्य से अभिव्यक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति की भूरि-भूरि प्रशंसा की। तदनन्तर श्रीधर आश्रम के चिकित्सालय में कुष्ठरोग का नियमित रूप से उपचार करने लगे। गुरुदेव इस नवदीक्षित शिष्य की इस असाधारण निष्ठा को आनन्दपूर्वक देखते थे। उन्होंने स्वयं उन कुष्ठियों को प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को भोजन कराने की व्यवस्था कर दी। युवक ब्रह्मचारी तथा अनुभवी गुरु की सदा एक ही मनोवृत्ति थी। जो रोगी आश्रम के विषम चिकित्सा (एलोपैथी) औषधालय में आते उन्हें ऐसा अनुभव होता कि डा. शिवानन्द जी की भाँति ही डा. राव जी भी रोगहरण की असाधारण शक्ति से सम्पन्न महात्मा हैं। डा. राव जी ने क्रियात्मक उपचार के लिए सतीशचन्द्र दास गुप्ता की 'होम ऐण्ड विलेज डाक्टर' (Home and Village Doctor) तथा राखाल दास गुप्ता की औषध-शास्त्र (Materia Medica) जैसी पुस्तकों पर पाण्डित्य प्राप्त कर लिया था। किन्तु वास्तविक महत्त्वपूर्ण बात तो यह थी कि वह उन बीमार रोगियों के प्रति अपना सच्चा प्रेम तथा निष्कपट चिन्ता प्रकट करते थे जो अब सुसोपाधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की अपेक्षा उनके आशीर्वाद को पसन्द कर बड़ी संख्या में आने लगे थे। 'डाक्टर का समय उसका अपना समय नहीं है' - इस सिद्धान्त-वाक्य पर चलते हुए श्रीधर अपने भोजन तथा विश्राम की उपेक्षा कर अपना सम्पूर्ण समय रोगियों के उपचार में लगाते थे। कभी-कभी उनका रोगहर स्पर्श चमत्कार करता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु की एक तमसावृत रात्रि में एक वृद्ध महिला अपनी छोटी पुत्री के साथ उनके सम्मुख उपस्थित हुई। उसकी पुत्री को एक विषैले वृश्चिक ने दंश लिया था। उन्होंने उसे तुरन्त ही अपने कुटीर में बुलाया और अपनी चोरबत्ती के प्रकाश से उसको मार्ग दिखाया। उनके पास लगाने के लिए कोई औषधि न थी। उन्होंने केवल अपने छोटे तौलिए को उसके आक्रान्त अंग पर मला और इस बीच ओष्ठों से भगवन्नाम उच्चारण करते रहे। लड़की तत्काल ही पीड़ामुक्त हो गयी। संवेदनशील डाक्टर द्वारा उत्पन्न प्रेम की शक्ति ऐसी थी कि विष ने भी अपनी विषाक्तता खो दी। उनकी करुणा सबको अपने में समाविष्ट करने वाली तथा अक्षय थी। उन्होंने इसे केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रखा अपितु पशुओं, पक्षियों तथा कीटाणुओं तक उसे विस्तारित किया था। एक दिन उन्होंने आश्रम के कार्यालय के पास एक कुत्ते को लेटा हुआ देखा। उसका शरीर व्रणों तथा कृमियों से भरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि वह कुछ समय से घोर व्यथा में था। राव स्वामी जी का कोमल हृदय इस करुणाजनक दृश्य से द्रवित हो उठा। उन्होंने कुछ औषधि खिलायी, सूई लगायी तथा प्रभावित अंगो की उचित रीति से मरहम-पट्टी की और सारी रात्रि उसकी सेवा-सुश्रूषा करते हुए उसके निकट सोये। आश्रमवासियों ने जब प्रात:काल इसे देखा तो वे स्तब्ध रह गये। गुरुदेव ने कहा कि राव स्वामी जी मानव नहीं वरन् करुणा के मूर्त रूप हैं। इस करुणामय व्यक्ति का ऐसा सद्भाव तथा ऐसी निष्ठा थी कि उसने लगभग दो माह तक अपने को उस कुत्ते की देख-रेख में लगाये रखा और जब तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गया तब तक उसे उन्मुक्त नहीं किया। गुरुदेव ने रहस्यमय ढंग से अपना मत अभिव्यक्त किया, "डा. राव तो डा. शिवानन्द से भी आगे बढ़ गये हैं।" डाक्टरों के इस डाक्टर ने, जो चिकित्सीय महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना ही औषधि-विशेषज्ञ बन गया, ग्राम-ग्राम में विचरण किया तथा पर्वतीय प्रदेश के जनसाधारण को चिकित्सीय सहायता प्रदान की। उन दिनों चिकित्सीय सुविधा के अभाव में बहुसंख्यक लोगों के प्राण चले जाते थे। ऐसे लोगों के लिए शिवानन्दाश्रम का यह सहानुभूतिशील ब्रह्मचारी साक्षात् धन्वन्तरि के रूप में प्रकट हुआ। उन दिनों राव स्वामी जी ने ऋषिकेश तथा उसके आस-पास के स्थानों में रोगियों के सेवा-काल में जो सदयता, समर्पण, विनम्रता तथा उदारता के उत्कृष्ट गुर्णो का प्रदर्शन किया, उसको पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए व्यक्ति को स्वर्गदूत की जिह्वा की आवश्यकता होगी। लोग जब कभी भी उनका गुणानुवाद करते तो सरल स्वामी जी विनम्रतापूर्वक कहते कि उन्होंने अपने गुरुदेव के जीवन से कुछ छोटी-छोटी बातें सीखी हैं। तत्पश्चात् वह जब स्वामी शिवानन्द गंगा-तट पर स्वयं साधना करते थे, उस समय की गुरुदेव की सेवाओं की कथाओं से, स्वर्गाश्रम में गुरुदेव के प्रारम्भिक जीवन से संकलित तथ्यों से उनका मनोरंजन करते थे। गुरुदेव किस प्रकार वयोवृद्ध महात्माओं तथा रोगियों के लिए गंगा से जल ला कर, उनके कमरों में झाडू लगा कर, उनके वस्त्र धो कर तथा उनके शौचालय तक की सफाई करके उनकी सेवा करते थे, इसका वर्णन वह बहुत ही भावपूर्ण ढंग से करते थे।
दैनिक साधना
श्रीधर अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनों से ही सत्य, विश्व-प्रेम तथा शुचिता के त्रियेक गुणों में प्रतिष्ठित थे। पूर्ण ब्रह्मचारी होने के कारण वह ओजस्-शक्ति से सदा कान्तिमय रहते थे। इसके अतिरिक्त, जो भी चर तथा प्राणधारी थे, उनमें भगवान् की सर्वव्यापकता के प्रति अनुक्रियाशील होने से वह सदा-सर्वदा प्रभु की उपासना में संलग्न रहते थे। अतः इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए दैनिक साधना की किसी अतिनियमनिष्ठ समय-सारिणी की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु वह तोतापुरी की प्रसिद्ध अभ्युक्ति को सदा स्मरण रखते थे कि पीतल के पात्र की चमक बनाये रखने के लिए उसे प्रतिदिन मलना होता है। गुरुदेव की भाँति वह भी इस बात पर बल देते थे : "शरीर सदा गर्दभ और मन अन्तिम दिवस तक मर्कट बना रहता है; अतएव आध्यात्मिक चाबुक तथा तितिक्षा, तपस्या आदि की छड़ी को सदा तैयार रखना चाहिए।" इसी भाँति गुरुदेव जो प्रायः चेतावनी दिया करते थे : "भले ही आप जीवन्मुक्त हों, परन्तु आपको सावधान रहना चाहिए।" इस बात में भी वह उनके साथ एक मत थे। 'राव स्वामी जी एक जन्मजात सिद्ध है' - ऐसा गुरुदेव का विचार था। तथापि वह अपने को सदा ही एक अनभ्यस्त, आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी-अभी प्रवेश करने वाला व्यक्ति ही मानते थे। अतएव वह समय-समय पर उपवास, आकस्मिक आत्म-दमन तथा तितिक्षा का आश्रय लिया करते थे।
तितिक्षा एक ऐसा गुण था जिसे श्रीधर ने आश्रम में आने से पूर्व ही अध्यवसायपूर्वक सम्पोषित किया था तथा जिससे वह प्रचुर मात्रा में सम्पन्न थे। तथापि ऐसा कोई भी दिन न व्यतीत होता जब वह अपने को किसी-न-किसी कठोर परीक्षा का विषय न बनाते; क्योंकि तितिक्षा संन्यासी की सच्ची सम्पत्ति है। भगवान् गीता में साधक को प्रेरित करते हैं कि 'सुख तथा दुःख, शीत तथा उष्ण को समचित्तता से सहन करो; क्योंकि वे भी अनित्य हैं।' राव स्वामी जी को एक ऐसे व्यक्ति के, अपने गुरु शिवानन्द के सान्निध्य में रहने से अतिरिक्त प्रेरणा प्राप्त थी जो अनुकरणीय जीवन्त तितिक्षु थे। गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रारम्भिक दिनों में ही अपने तितिक्षा-गुण के लिए प्रख्यात थे। शिवानन्द अपनी साधना में कोई अवरोध न आये, इसके लिए प्रतिदिन स्वल्प आहार के लिए अन्नक्षेत्र न जा कर, बासी रोटी के टुकड़े संग्रह कर रखते और उस पर ही अपना निर्वाह करते तथा लगातार कई दिनों तक ध्यान करते रहते थे। इस भाँति वह अपने पास कुछ सूखी चीमट रोटियाँ रखने के अभ्यस्त थे और जब कभी भूख लगती तो उसे गंगाजल में भिगो कर खा लेते थे जिसका अर्थ यह हुआ कि वह एक दिन के भोजन पर एक सप्ताह तक निर्वाह करते थे। तितिक्षा के इस गुण ने, जिसे गुरुदेव ने उस समय भी बड़ी सावधानीपूर्वक बनाये रखा था, राव जी पर गम्भीर प्रभाव डाला जिन्होंने, जैसा कि हम 'आलोक-पुंज' (Light Fountain) से समझते हैं, गुरुदेव के आन्तर जीवन के पृष्ठों को पूर्ण मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया था। गुरुदेव का जीवन कोई गुप्त विषय नहीं था। वह सर्वविदित था; किन्तु श्रीधर की भाँति सच्चे विवेक तथा समझ के स. थ उसका अध्ययन कर सकने वाले लोग बहुत ही कम थे और ऐसे लोगों की संख्या तो और भी कम थी जो उसके अध्ययन से लाभ उठा सके। गुरुदेव के स्वर्गाश्रम के प्रारम्भिक जीवन से, जैसा कि उनके सेवकों से हमें ज्ञात हुआ है, राव स्वामी जी इतना अनुप्राणित हुए कि उन्होंने अपने शरीर को, जो सुख-साधनों में पला था, सच्ची शिक्षा देने का विचार किया। ऐसा सोच कर वह शिशिर ऋतु की रात्रि में अपने कुटीर से बाहर आ गये और उषा-काल आने तक आच्छादन-वस्त्र के बिना बैठे रहे। वह भी इस अवस्था में, जब कि तीक्ष्ण शीत वायु हड्डियों तक को कम्पायमान करती हुई उनके झुर्रीदार शरीर से टकरा कर बह रही थी, शान्त बने रहे। इस भाँति उन्होंने तपस्या की ज्वाला को सुस्थिर तथा अविरत बनाये रखा।
स्वामी जी आश्रम के अपने प्रारम्भिक आवास-काल में एकान्त स्थलों में जप तथा ध्यान में लगातार घण्टों तक निमग्न रहते। वह गंगा के दूसरे तट पर स्वर्गाश्रम से लगभग सात मील दूर तथा उत्तुंग मणिकूट-पर्वत के उस पार नीलकण्ठ महादेव के मन्दिर के दुष्कर आरोह पर प्रायः चले जाते और उसकी एकान्त शान्ति में गम्भीर ध्यान में निमग्न हो जाते और काल-प्रवाह का अतिक्रमण कर समाधि में चले जाते थे। वह कभी-कभी ब्रह्मपुरी को अपनी तपस्थली के लिए चुनते। उस स्थान में एक गुहा है जिसमें स्वामी रामतीर्थ कठोर तपस्या किया करते थे। यह स्थान सुगम्य नहीं है; क्योंकि सर्पों तथा हिंस्र पशुओं से बाधित है। स्वामी जी इस प्रकार के पवित्र किन्तु दूर स्थानों में, मानव-आवास से बहुत दूर अपनी उच्चतर साधना किया करते थे। गुरुदेव की अनुमति से वह आन्तरिक शान्ति तथा नीरवता की खोज में फूलचट्टी अथवा गरुड़चट्टी जाया करते थे। वह जीवन-निर्वाह हेतु अपने साथ द्रव आहार ले जाते और वहाँ कई दिनों तक निरन्तर ध्यान करते थे। एक तितिक्षु साधु ने जो अपनी असाधारण कठोर तपस्या के लिए प्रख्यात थे तथा अपने शरीर को आच्छादित करने के लिए केवल टाट के टुकड़े पहनने के कारण 'टाटवाला' पदवी प्राप्त किये थे, बाद में बतलाया कि उन्होंने बहुधा स्वामी जी को कठोर कष्ट झेल कर तप तथा ध्यान करते हुए देखा था। इस लेखक को स्वामी ध्यानानन्द जी से ज्ञात हुआ कि एक टाटवाले तपस्वी ने, जो भूतनाथ-गुफा में लगभग तीस वर्ष तक रहे थे, एक बार स्वामी जी के कुछ भक्तों को बतलाया कि स्वामी जी ब्रह्मचारी की अवस्था में शान्त ध्यान के लिए उस गुफा में आया करते थे। उस तपस्वी ने यह स्वीकार किया कि उन प्रारम्भिक दिनों में भी इस युवक ब्रह्मचारी की अनुकरणीय विनम्रता, दयालुता तथा निर्भयता के कारण उनमें उसके लिए श्लाघा का गम्भीर भान्न था। इस भाँति दीर्घावधि के गम्भीर ध्यान के अनन्तर आश्रमवासी साथियों के साथ निरन्तर कठोर श्रम की अवधि आती रहती।
उन्होंने बड़े ही सूक्ष्म ध्यान से अवलोकन किया कि गुरुदेव किस प्रकार लोक-संग्रह के हित में अपनी गतिकता का प्रबल प्रवृत्तियों के बावजूद भी अपने अन्दर वैराग्य की अग्निशिखा को अविरत जलाये हुए अन्तर में सदा विरक्त संन्यासी थे। उन्होंने देखा कि गुरुदेव उन सबके मध्य शरीर से सदा उपस्थित रहते हुए भी समय-समय पर पूर्ण आभ्यन्तरता की ऐसी अवस्था में चले जाते थे कि व्यक्ति को यह दावा करना कठिन हो जाता कि वह वहाँ वास्तव में उपस्थित थे। यह निश्चय ही शास्त्रों में वर्णित विलक्षण 'निष्प्रपंचावस्था' थी। उन्होंने यह भी देखा कि गुरुदेव द्वन्द्वातीत, अतिवर्णाश्रमी तथा वर्णहीन स्फटिक होते हुए भी अपने बहुमुखी व्यक्तित्व से बहुत ही सुयोग्य बीस युवक संन्यासियों को प्रभारित तथा आबद्ध रखते थे। गुरुदेव जब अपने कुटीर से बाहर निकलते तो वह प्रेरित करते, मार्गदर्शन करते तथा कार्य करते हुए गुरुगोविन्दसिंह बन जाते और जब अपने कुटीर में होते तो वह अपनी 'सहजावस्था' में तल्लीन गुरु नानक का रूप ले लेते थे।
यह पाठ राव स्वामी जी ने अपने गुरुदेव के जीवन से सीखा। गुरुदेव की भाँति ही वह प्रातः से रात्रि होने तक प्रवृत्तियों में अविरत संलग्न रहने के बावजूद 'शान्त समाहित चित्त' पर जिसमें व्यक्ति भागवत सत्ता के साथ संलाप करता है, सदा अपना वैसा अधिकार रखते थे जैसा कि आज भी रखते हैं। इनके घनिष्ठ मित्र तथा एक परमोच्च कोटि के उन्नत ज्ञानयोगी स्वामी कृष्णानन्द जी इनकी इस अवस्था को पहचान सके जिसमें राम के अतिरिक्त अन्य कुछ न था- 'सर्वं राममयं जगत्' -इस अनुभूति से ही राव स्वामी जी की सभी प्रवृत्तियाँ अनुप्राणित होती थीं और वह विनम्रता के साक्षात् अवतार ही प्रतीत होते थे। वह सदा-सर्वदा सबके साथ अब तृण-पत्र की भाँति विनम्र, प्रशान्त तथा अनात्मशंसी-सा रहते। स्वामी कृष्णानन्द जी जैसे व्यक्ति ही अपने उन्नत योग के धरातल से अपने वरिष्ठ गुरुभाई की उन्नत आध्यात्मिक स्थिति का सम्यक् मूल्यांकन कर सके और उनमें से अनेक लोगों ने, युवक राव स्वामी जी उस समय आध्यात्मिकता के जिस असाधारण शिखर पर पहुँच चुके थे, उसे बतलाया। गुरुदेव के लिए अपने इस सर्वाधिक प्रिय शिष्य की अद्वितीय उन्नतावस्था का मापना निस्सन्देह सरल था। उन्होंने बहुत शीघ्र ही घोषित किया: "राव स्वामी जी को सभी कार्यों से मुक्त कर देना चाहिए; किन्तु मैं चाहता हूँ कि वह महासचिव के महान् पद को सँभाल लें। ऐसे महान् सन्त को अपना महासचिव बनाना स्वयं संस्था के लिए परम गौरव का विषय है।"
संन्यास-दीक्षा
इस अवस्था में यह स्मरणीय है कि स्वामी जी अभी तक गैरिक परिधान नहीं धारण किये थे। तथापि बड़े-बड़े महात्मा इनका सम्मान करते थे। वे इनके चरणों में सहज ही नतमस्तक होते थे। रोगियों की निष्काम सेवा द्वारा इन्होंने अड़ोस-पड़ोस के लोगों का प्रेम, श्लाघा तथा कृतज्ञता अर्जित कर ली थी और अब इन्होंने अपने आध्यात्मिक उत्साह तथा ज्ञान के द्वारा ऋषिकेश के महात्माओं का सम्मान प्राप्त कर लिया। किन्तु इन सबके होते हुए भी स्वामी जी बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा करते थे कि वह अभी केसरिया परिधान धारण करने योग्य नहीं हैं। फिर भी गुरुदेव ने श्रीधर पर स्वामी चिदानन्द-आनन्द तथा प्रबोध में सदा संस्थित- इस उपयुक्त नाम के साथ महान् त्याग का चिह्न इन्हें प्रदान करने की आनन्दप्रद प्रेरणा अनुभव की। गुरुदेव सदा गाया करते थे :
"चिदानन्द चिदानन्द चिदानन्द हूँ।
हर हाल में अलमस्त सच्चिदानन्द हूँ।"
वह चिदानन्द के साथ अपने को अभिन्न समझते थे और तदनुसार ही उन्होंने अपने परम प्रिय शिष्य का नामकरण किया। इस नवयुवक संन्यासी के लिए, जिसने ऐसा लगता है कि बहुत समय पूर्व ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, यह नवीन संन्यासी नामपट्ट एक विधिवत् स्वीकृति मात्र थी। इस भाँति परम पवित्र गुरुपूर्णिमा- दिवस-१० जुलाई १९४९ - को जो दिव्य जीवन संघ तथा विश्व के तिथिपत्र में एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दिवस था, एक बहुत ही महत्त्व के धार्मिक संस्कार में श्रीधर ने, इह तथा अमुत्र लोकों के सुखों का न्यास कर सरस्वती-परम्परा के पवित्र संन्यासाश्रम में प्रवेश किया। जब श्रीधर ने विरज-होम किया और यज्ञाग्नि में अपने पूर्वाश्रम की आहुति डाली तथा स्वामी चिदानन्द सरस्वती नया नाम धारण कर ब्रह्मविद्या-गुरुओं की शृंखला में अपने को संयुक्त किया तो स्वयं यह (संन्यास) आश्रम उन्हें अपने में सम्मिलित करके महिमान्वित हो गया।
जीवन्मुक्त आत्मा
आवश्यकता की माँग के अनुसार तीव्र प्रवृत्तियों के बावजूद अब से आगे स्वामी जी के जीवन का सुदृढ़ आधार अविच्छिन्न ध्यान था। अपने उपलब्ध प्रत्येक अवसर का लाभ उठा कर वह निर्जन स्थानों में चले जाते तथा आन्तरिक मौन तथा समाधि में निमग्न रहते। ऐसे ही एक अवसर पर मध्याह्नोपरान्त किसी समय आश्रम से प्रस्थान किया और लक्ष्मण-कुण्ड लगभग ३-३० बजे पहुँचे। वह वहाँ अपनी चेतना को रोक कर सहज स्वाभाविक रूप से गम्भीर ध्यान में निमग्न हो गये। बहुत शीघ्र ही उन्होंने अपने को अतिचेतनावस्था में उन्नीत हुआ अनुभव किया जहाँ मन पूर्णतया विनष्ट हो जाता है। वह सायंकाल को बहुत विलम्ब से, लगभग ९ बजे रात्रि में अपनी सामान्य भौतिक चेतना में वापस आये। उस समय निविड़ अन्धकार था; किन्तु स्वामी जी अलौकिक आनन्द से इतना अधिक आपूरित थे कि वह भयावह रात्रि भी उन पर कुछ प्रभाव न डाल सकी और वह लगभग अर्धरात्रि को ही दबे पाँव आश्रम वापस आये।
स्वामी चिदानन्द आश्रम में गुप्त निधि के रूप में और अधिक समय तक न रह सके। उनके दिव्य जीवन की सुरभि ने उनके वातावरण को सुवासित कर दिया तथा वह सर्वत्र फैल गयी। इसके पश्चात् जिस किसी ने भी इन्हें देखा, उसने इनके शरीर के चतुर्दिक् कुछ असाधारण चुम्बकीय तथा द्युतिमान् पाया। निश्चय ही यह महान् घटना स्वयं गुरुदेव को, जो एक बहुत ही उच्च कोटि के भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त सन्त थे, स्पष्ट ज्ञात थी। स्वामी शिवानन्द ने निस्संकोच घोषित किया कि 'स्वामी चिदानन्द का वर्तमान जीवन उनका अन्तिम जन्म है।' उन्होंने अपने शिष्यों से कहा: "चिदानन्द एक सन्त हैं। आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। वह आपके गुरु हैं।" गुरुदेव के प्रमुख शिष्यों को भी स्वामी चिदानन्द की मुक्त स्थिति को जानने में अधिक समय नहीं लगा। उदाहरणार्थ : गुरुदेव के वरिष्ठ शिष्य तथा दिव्य जीवन संघ के प्रथम महासचिव स्वामी परमानन्द जी ने स्वामी चिदानन्द जी में जो उनके मुक्तात्मा सन्त का स्वरूप देखा, उसका सुन्दर चित्र प्रस्तुत कर उन्होंने इस तथ्य को आश्रमवासियों को भली प्रकार समझाया। आइए, हम इस महान् साधक के शब्दों को सुनें, "मैंने उन्हें बिल्लियों, कुत्तों तथा बन्दरों को खाना खिलाते तथा उनकी सेवा करते देखा है। आश्रम जब आर्थिक संकट में है, उस समय वह मूल्यवान् सूइयाँ लगा कर एक रुग्ण कुत्ते के उपचार में प्रचुर धन व्यय कर रहे हैं। जब सैकड़ों पत्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह स्थानीय बालक तथा बालिकाओं को उपदेश दे रहे हैं और उन्हें मिष्टान्न, बिस्कुट तथा फल दे कर तुष्ट कर रहे होंगे। जब उन्हें अपने निजी कार्य में हाथ लगाने का समय न होगा, वह एक रोगी को सन्तुष्ट करने अथवा एक कीड़े अथवा मनोहर पुष्प की प्रशंसा में घण्टों व्यय कर देंगे।... मैं अनुभव करता हूँ कि यदि मेरे पास स्वामी चिदानन्द जी के ज्ञान, क्षमता तथा गुरुदेव के चरण-कमलों में भक्ति का सहस्रांश भी होता तो गुरुदेव के निकट सम्पर्क में जो इतने दिन मैंने व्यतीत किये, उससे मैं प्रख्यात त्रोटकाचार्य की स्थिति प्राप्त कर लिया होता।" गुरुदेव के एक अन्य ज्ञानवृद्ध शिष्य स्वामी हरिशरणानन्द जी ने भी उनका ध्यान इसी विषय की ओर आकृष्ट किया-"स्वामी चिदानन्द जी बिल्लियों तथा बन्दरों तक की अन्त्येष्टि करते हैं, मन्त्र पढ़ते तथा कीर्तन करते हैं। यह निष्काम सेवा है। यह उत्कृष्ट विश्व-प्रेम है। चिदानन्द जी इस भावना से पूर्ण हैं कि जो भी उनके सम्पर्क में आता है, वह नारायण है।" श्री नारायण स्वामी जी ने चिदानन्द जी की उपलब्धियों का समाहार प्रस्तुत किया और कहा : "संक्षेप में कहें तो वह अनेक कलाओं में निपुण हैं। वह आदर्श साधक, आदर्श शिष्य तथा रोगियों तथा निर्धनों के सच्चे मित्र हैं। वह एक दार्शनिक हैं, राजयोगी हैं तथा एक सन्त हैं।" गुरुदेव के समय में आश्रम के प्रख्यात पुरावृत्त लेखक स्वामी वेंकटेशानन्द जी ने सन् १९५४ में बधाई देते हुए स्वामी चिदानन्द जी को निम्नांकित शब्दों में सम्बोधित किया: "वह देश धन्य है जिसने आप जैसे एक महापुरुष को जन्म दिया। वे लोग धन्य हैं जिन्हें आपके सत्संग का, भले ही एक क्षण के लिए, सुख भोगने का सद्भाग्य प्राप्त है। वह युग धन्य है जिसमें आपने इस धराधाम पर अवतरित होने का समय चुना है।"
स्वामी जी के जीवन का प्रभामण्डल, महान् गुरुदेव के प्रकट प्रख्यापन तथा अगण्य महात्माओं के साक्ष्य-ये सब दृढ़तापूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँचाते हैं कि इस पार्थिव जगत् में उनका वर्तमान प्रवास एक जीवन्मुक्त आत्मा का है। उन्होंने ठीक किस दिन परम आत्म-साक्षात्कार प्राप्त किया, यह विषय निस्सन्देह सदा एक रहस्य ही बना रहेगा। इस पुस्तक का लेखक इस विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वामी जी के पास गया; किन्तु स्वामी जी ने स्पष्ट कहा : "यह गुरुदेव तथा मेरे मध्य एक रहस्य है। मैं इस रहस्योद्घाटन के लिए प्राधिकृत नहीं हूँ।" वास्तव में, जब गुरुदेव शिवानन्द से इस विषय का प्रश्न किया गया तो उन्होंने भी इस प्रकार का उत्तर दिया था और आगे कहा था कि इस विषय में कुछ कहने के लिए श्रुतियों ने निषेध किया है। स्वामी चिदानन्द जी के विषय में तो यह बात विशेषकर है कि उनसे उनकी किसी भी महान् उपलब्धि का महत्त्व दिलाना प्रायः असम्भव ही है। जब भी उनसे अपना मत प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जाता है तो विषय की दिशा मोड़ कर इसे वह किसी-न-किसी की प्रशंसा की भरमार करने के अवसर के रूप में बदल देते हैं और स्वयं को कुशलतापूर्वक केन्द्र-बिन्दु से हटा लेते हैं। एक प्रादेशिक दिव्य जीवन सम्मेलन में किसी भक्त ने सच्चे तथा गम्भीर उत्साह से इनसे प्रश्न किया, "मैं किसी साक्षात्कार-प्राप्त आत्मा से दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवन्! क्या आप भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त आत्मा हैं।" स्वामी जी ने उत्तर दिया : "मैं तो गुरुदेव का एक सेवक और भगवान् का एक अयोग्य दास मात्र हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मैं भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त आत्मा हूँ अथवा नहीं। यह तो केवल भगवान् ही जानते हैं।" केनोपनिषद् ने यह सुस्पष्ट कहा है कि भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त ऋषि में किंचिन्मात्र भी अभिमान नहीं रहता कि वह घोषित करे कि उसने भगवान् का साक्षात्कार कर लिया है। श्रुतियों के प्रकाश में स्वामी जी के उपर्युक्त शब्द उन्हें न केवल एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों से सम्पन्न व्यक्ति अपितु एक ऐसा व्यक्ति भी सूचित करते हैं जिसने भगवान् तथा गुरुदेव के चरणों में अपनी आत्मा-सहित अपना सर्वस्व पूर्णतया अर्पित कर दिया है।
स्वामी जी ने उन दिनों आश्रम-जीवन से स्थायी रूप से अलग हो कर सर्वशक्तिमान् प्रभु के हाथों में सब-कुछ छोड़, सब चिन्ताओं से मुक्त हो कर एकान्तवासी का, एक परिव्राजक संन्यासी का जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया था। उनके ये आन्तरिक विचार छोटे-बड़े सैकड़ों अवसरों पर व्यक्त हुए थे। उन्होंने परवर्ती काल के अपने एक पत्र में अपनी मनोदशा का वर्णन इस प्रकार किया : "मेरी सम्पूर्ण सत्ता एकान्त तथा एकाकी चिन्तन तथा अन्तर्मुखी जीवन की ओर अत्यन्त आकृष्ट थी। सन् ५६ से ही मैं उस मार्ग की ओर प्रेरित होता जा रहा था।" उनके जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण, उनके व्यक्तित्व में कुछ लक्षणों का सुस्पष्ट रूप से विकास उनके गुरुदेव तथा साथी साधकों के कथन तथा अनेक भक्तों का साक्ष्य-ये सभी इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि सन् १९५४ में जब उनका उनतालीसवाँ जन्मदिवस मनाया गया, उस समय यह एक पूर्ण स्फुटित ज्ञानी, सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों से सम्पन्न प्रबुद्ध आत्मा थे। अतएव, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुरुदेव शिवानन्द ने स्वयं घोषित किया कि स्वामी चिदानन्द अध्यात्म-ज्ञान-ज्योति तथा ब्रह्मसूत्र और गीता के मूर्तरूप हैं। वह अपने हृदय से उपनिषदों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने सबको प्रकट किया कि 'स्वामी चिदानन्द का वर्तमान जीवन उनका अन्तिम जन्म है।' उन्होंने तो यहाँ तक कहा: "मैं भी उन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देता हूँ।"
संस्था की सेवा
स्वामी जी ने अपने शिष्यत्व की दीर्घावधिभर एक महान् सूत्र का अनुसरण किया है- "गुरु-वाक्य वेद-वाक्य है।" वह सदा ही अहंभाव रहित 'वंशी' तथा गुरुदेव 'वंशीवादक' रहे हैं। उनके अपने जीवन में कोई स्पृहा न थी, कोई संस्था स्थापित करने का उनमें सत्संकल्प भी न था। शिवानन्दाश्रम से उनका सम्बन्ध पूर्णतया आध्यात्मिक था। सांस्थानिक विकास की उनमें कोई कामना न थी। यह सब-कुछ भगवदिच्छा थी जो दिव्य जीवन संघ का आश्चर्यजनक रूप से बहुमुखी तथा व्यापक विकास हुआ। आश्रम की उनकी सेवा अपने गुरु की अर्चना मात्र थी। सन् १९४३ में जब यह आश्रम मैं सम्मिलित हुए तो यह उन प्रतिष्ठित साधकों में प्रमुख अभिनेता थे जिन्होंने अपने अथक प्रयास तथा भारतवर्षभर में गुरुदेव के विचारों के प्रक्षेपण द्वारा उनकी संस्था की ध्वजा को ऊपर उठाया। स्वयं गुरुदेव अपने इस नवप्राप्त शिष्य की आश्चर्यजनक क्षमता को शीघ्र ही जान गये थे। आश्रमवासी भी तत्काल ही पूर्ण रूप से समझ गये कि स्वामी चिदानन्द जी गुरुदेव की ही प्रायः प्रतिकृति हैं। पाँचवें दशक में ही गुरुदेव ने युवक ब्रह्मचारी श्रीधर राव की ओर निर्देश करते हुए अपने एक वृद्ध सज्जन भक्त मेजर जेनरल ए. एन. शर्मा से कहा था, "मेरा उत्तराधिकारी आ गया है।" युवक ब्रह्मचारी अपनी ओर से गुरुदेव के आह्वान के प्रति पूर्णतया प्रतिक्रियाशील थे। सूक्ष्म निरीक्षण, आन्तरिक विनिमय तथा बारम्बार के ध्यान ने उन्हें गुरुदेव के विचारों तथा आन्तरिक आकांक्षाओं के प्रति आश्चर्यजनक रूप से अतिसंवेदनशील तथा जागरूक बना दिया था। इनकी 'लाइट फाउण्टेन' (Light Fountain-आलोक-पुंज) -अपने गुरुदेव की जीवनी-सम्बन्धी कृति जिसका सभी जिज्ञासु पाठक एक अद्वितीय आध्यात्मिक प्रलेख के रूप में सदा परिशीलन करेंगे-उस गम्भीर मूल्यांकन का रोमांचक साक्ष्य देता है। यह जीवनचरित-सम्बन्धी रचना पाण्डित्यपूर्ण है तथा शैली की प्राजंलता, श्रुति-मधुर शब्द-योजना तथा अपने प्रतिपाद्य विषय के गम्भीर ज्ञान के कारण अपनी विशिष्टता रखती है। इसके प्रस्तुतिकरण का पूर्णतया विनीत भाव पाठक को इसके पृष्ठों में सदा ही शिवानन्द के दर्शन कराता है, लेखक का नहीं। स्वयं गुरुदेव इस पुस्तक में अन्तर्विष्ट आध्यात्मिक उत्साह तथा ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा: "शिवानन्द महाप्रयाण कर जायेंगे, किन्तु 'लाइट फाउण्टेन' (आलोक-पुंज) टिका रहेगा।" सन् १९४४ में पुस्तक का उन्मोचन करते समय स्वामी जी ने कृतक नाम 'प्रिज्म' (Prism क्रकच) के अन्तर्गत कर्तृत्व को गुप्त रखना पसन्द किया। चिदानन्द वास्तव में पवित्र 'प्रिज्म' (क्रकच) हैं जिसके माध्यम से गुरुदेव ने जगत् के हित के लिए अपने बहुमुखी व्यक्तित्व को प्रकट करना पसन्द किया।
अतः आश्रम के सभी लोग चिदानन्द को सभी विषयों में गुरुदेव का प्रतिनिधि समझने लग गये। वही सभी विशेष समारोहों में मुख्य वक्ता होते थे। आश्रम में प्रतिष्ठित अभ्यागतों तथा जिज्ञासुओं के समक्ष वह गुरुदेव के आदर्शों के उपयुक्त व्याख्याता थे। वह इस प्रक्रम में सदा ही नवागत को गम्भीर रहस्य का, ऋषियों के कुछ गूढ़ ज्ञान का दिग्दर्शन कराते। गुरुदेव ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था कि 'चिदानन्द जी ने अपने सभी भावपूर्ण प्रवचनों में किसी बौद्धिक पद्धति से मूल-पाठ को हाथ में न ले कर उपनिषद् के गूढ़ ज्ञान को प्रस्तुत किया है।' कभी-कभी वह अपने को अप्रकट रख कर 'डिवाइन लाइफ' मासिक पत्रिका के पृष्ठों को समृद्ध बनाते थे। उनके छद्यनाम 'कौशिक' से प्रकाशित 'स्वामी शिवानन्द वर्तमान परिप्रेक्ष्य में-एक अध्ययन', 'महज्जन' जैसे भावोद्दीपक लेख अध्यात्म के मौलिक विषय थे। उन दिनों में दिये गये उनके बोधप्रद अधिकांश भाषणों को स्वामी वेंकटेशानन्द जी ने संकलित किया जो बाद में 'योग पर आरण्य-विद्यापीठ में भाषण' शीर्षक से प्रकाशित हुए। स्वयं गुरुदेव उन भाषणों से इतना अधिक प्रभावित हुए कि इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के उपोद्घात में इस रचना का उल्लेख करते हुए लिखा "एक महान् सन्त तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शक स्वामी चिदानन्द के अत्यन्त प्रेरणाप्रद भाषणों का रोमांचक ग्रन्थ। इन भाषणों में जीवन के सभी विषय समाविष्ट हैं और मुझे इसमें किंचित् भी सन्देह नहीं है कि इस ग्रन्थ का प्रकाशन हमारे प्राचीन धर्म, संस्कृति तथा जीवनविधा के परिरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करेगा।"
स्वामी जी ने योग-वेदान्त-अरण्य-विश्वविद्यालय (अब विद्यापीठ) के माध्यम से, जहाँ गुरुदेव ने इन्हें राजयोग का प्राध्यापक नियुक्त किया था, अपने को अध्यात्म-ज्ञान के प्रसार के लिए, योगशास्त्र के गूढ़ अर्थ तथा व्यावहारिक उपयोग के लिए समर्पित कर दिया। अनेक ज्ञानवृद्ध शिष्यों ने इस संस्था की सफलता के लिए अपना योगदान दिया, किन्तु स्वामी चिदानन्द तथा स्वामी कृष्णानन्द विश्वविद्यालय के मार्गदर्शक प्रकाश थे। चिदानन्द नीचे द्रुतगामिनी तथा वैभवशालिनी गंगा के बालुकामय तट पर जाने वाली पहाड़ी की ढाल पर वृक्षहीन क्षेत्र में स्थित इस विश्वविद्यालय को एक अद्वितीय आध्यात्मिक शिक्षण-संस्थान समझते थे। गुरुदेव ने इन्हें राजयोग के प्राध्यापक होने के साथ-साथ इसका प्रथम कुलपति नियुक्त किया। चिदानन्द के पाण्डित्यपूर्ण भाषण सुनने के लिए छात्रों को सदा प्रतीक्षा नहीं करनी होती थी। चिदानन्द का जीवन ही उनके लिए सर्वोत्कृष्ट पाठ था। वस्तुतः योग का एक विचारशील छात्र दूर से ही उनके जीवन का अवलोकन करके नैतिक अनुशासन, मनोजय तथा अतिचैतन्यावस्था की अनुभूति के विषय में बहुत अधिक सीख सकता है। स्वामी जी सहस्रों लोगों की सभा की अध्यक्षता करते समय भी अपने मुखमण्डल से दिव्य आभा विकिरण करते हुए प्रत्याहरण कर प्रायः गम्भीर ध्यानावस्था में जा पहुँचते हैं। सक्रिय सेवा में संलग्न रहते समय भी वह सदा पर-वैराग्य तथा उग्नामक्ति में प्रतिष्ठित रहते हैं।
राजयोग पर उनके भाषण अपरोक्षानुभूति पर आधारित थे और इसलिए अत्यधिक प्रभावशाली थे। इसी भाँति वेदान्त के प्राध्यापक स्वामी कृष्णानन्द अपने छात्रों के मस्तिष्क में उपनिषद् की विचारधारा उत्पन्न करने वाली एक प्रभावशाली शक्ति थे। वह स्वयं ज्ञानयोग के साधनचतुष्टय के निदर्शन थे। इन दोनों आध्यात्मिक धीर पुरुषों के विषय में गुरुदेव ने एक बार कहा था, "जरा उस ज्ञान को देखें जिससे चिदानन्द जी तथा कृष्णानन्द जी सम्पन्न हैं। राजा तथा राष्ट्रपति इनके चरणों में नतमस्तक होंगे। संसार उनकी चरण रज को सम्मान देगा। आप सबको उनकी चरण-रज लेनी चाहिए और उसे बहुत ही श्रद्धा तथा भक्ति के साथ अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। कितनी अल्पवयस् में उन्होंने संसार का त्याग किया है! उनमें ज्ञान की उत्कण्ठा की गहराई कितनी होगी! उनमें वैराग्य की तीव्रता कितनी होगी! संसारभर के लोग दर्शन तथा योग के मूल सिद्धान्तों को सीखने के लिए चिदानन्द जी तथा कृष्णानन्द जी जैसे व्यक्तियों के चरणों में पड़ेंगे। वे सच्चे सम्राट् हैं।"
योग के एक अन्य धृतिमान् योगी स्वामी हरिशरणानन्द जी अपने वैयक्तिक उदाहरण तथा निर्देश-दोनों ही प्रकार से भक्तियोग की पद्धति की शिक्षा देते थे। अद्वितीय हठयोगी स्वामी विष्णुदेवानन्द जी हठयोग का प्रशिक्षण देते थे। अन्य अनेक व्यक्ति थे जो इस काम में सहभागी बने। इनमें स्वामी चिन्मयानन्द जी, स्वामी वेंकटेशानन्द जी, स्वामी सत्यानन्द जी तथा स्वामी शाश्वतानन्द जी उल्लेखनीय हैं। इन सभी लोगों ने विद्यापीठ की अमूल्य सेवाएँ कीं। स्वामी हरिशरणानन्द जी ने एक बार अतीत के उन सुखमय दिनों को स्मरण करते हुए कहा था कि सन् १९४५ से १९५७ के बारह वर्ष फिर कभी नहीं दिखायी पड़ेंगे। ये वे महत्त्वपूर्ण दिन थे जब शिवानन्दाश्रम का योग-साधना-कुटीर समर्पित साधकों से भरपूर था-कमरा नं. १ तथा २ में स्वामी चिदानन्द, कमरा नं. ३ में स्वामी कृष्णानन्द, कमरा नं. ४ में स्वामी हरिओमानन्द, कमरा नं. ५ में स्वामी शाश्वतानन्द, इसी भाँति नामों की एक लम्बी सूची है। चिदानन्द सन्त-विद्वानों की इस असाधारण टोली के अग्रणी थे।
उन्होंने प्रारम्भ में पतंजलि के योगसूत्रों का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। उन भाषणों में से कुछ भाषण उनकी पुस्तक 'योग' में समाविष्ट किये गये और बाद में सम्पूर्ण प्रवचनों में से अधिकांश 'पाथ टू ब्लेसेडनेस' (Path To Blessedness - महान् जीवन की पथ-प्रदर्शिका) नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। उन ब्रह्मचारियों का निश्चय ही परम सद्भाग्य था जिन्होंने उनके प्रवचनों को एकान्तर दिवस को ब्राह्ममुहूर्त-वर्ग में एक वर्ष से अधिक समय तक सुना।
कार्यालय, कक्षा तथा पड़ोस के सब कार्य जैसे कि उनके लिए पर्याप्त न हों, उनके कन्धों पर और अधिक कर्तव्यों का ढेर लगा दिया गया। एक दिन रात्रि को लगभग १० बजे संयोग से जब वह गंगा के तट पर इधर-उधर घूम रहे थे, उन्होंने गुरुदेव को अपने कुटीर से बाहर आते देखा। गुरुदेव नारायण स्वामी जी के पास गये जो उस समय कुछ वस्त्र धो रहे थे। उन्होंने कहा- "हम केवल एक ही मासिक पत्रिका प्रकाशित करते हैं। एक साप्ताहिक अथवा एक दैनिक पत्रिका भी आरम्भ करें।" कोषाध्यक्ष स्वामी जी ने कहा: "डाक-शुल्क पर बहुत अधिक व्यय पड़ेगा।" गुरुदेव का सरल-सा उत्तर था : "भगवान देंगे। इसे अभी आरम्भ करें।" ऐसा कह कर उन्होंने चिदानन्द जी तथा अन्य स.धों को अकर्मण्य साधकों पर आशु तथा तात्क्षणिक क्रिया करने वाले दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक अन्तःक्षेप शिवानन्द- प्रयोगशाला में तैयार करने के कार्य में लग जाने का आदेश दिया। इस भाँति एक दैनिक पत्रिका (बुलेटिन) प्रारम्भ की गयी जो अनुलिपित्र (ड्यूप्लिकेटर) में मुद्रित होती थी। 'ज्ञानसूर्य-माला', 'केन-माला', 'योग-वेदान्त फ़ारेस्ट यूनीवर्सिटी', 'विज़डम लाइट', 'हेल्थ एण्ड लाँग लाइफ', 'ब्रांच गजट', 'डिवाइन लाइफ', 'योग-वेदान्त' तथा 'आरोग्य जीवन' नामक पत्रिका-समूह अरण्य विश्वविद्यालय की निहाई से प्रकट होने वाले आध्यात्मिक स्फुलिंग थे।
स्वामी चिदानन्द जी इन सभी नानाविध कार्यों के मध्य में भी सनातन सत्यों में नूतनता लाने तथा उन्हें अनूठे तथा रोचक रूपों में प्रक्षेपित करने को सदा उत्सुक रहते थे जिससे कि साधारण लोग समन्वय-योग के मार्ग की ओर आकृष्ट हो सकें। उदाहरणार्थ, उन्होंने एक आध्यात्मिक संग्रहालय स्थापित करने का विचार व्यक्त किया जिससे कि योग के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषयों को विविध प्रतीकों, पुस्तकों तथा चित्रों द्वारा रोचक ढंग से प्रक्षेपित किया जाय और उन्हें प्रशिक्षित पथ-प्रदर्शक जिज्ञासु अभ्यागतों को महाकक्ष में दिखलाये। वह चाहते थे कि संग्रहालय का निरीक्षण साधना का एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम बन सके। योग से अपरिचित लोगों के लाभार्थ संग्रहालय को आकार देने के लिए स्वामी जी ने स्वयं सोत्साह आवश्यक सामग्री संग्रह की तथा उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया। इसमें राजयोग, हठयोग, कुण्डलिनीयोग, जपयोग तथा तन्त्रयोग के जटिल पाठों को चित्रात्मक प्रतिरूपों की सहायता से स्पष्ट किया गया था। इस भाँति सन् १९४७ में योग-संग्रहालय का जन्म हुआ। यह विशिष्ट आध्यात्मिक भोजन प्रथम भजन हाल में सँजोया गया और बाद में एक अन्य महाकक्ष में स्थानान्तरित कर दिया गया जो योग-संग्रहालय-महाकक्ष के नाम से विख्यात हुआ। यह शिक्षा के साथ-साथ आनन्द का स्रोत था।
सन् १९४७ के दिसम्बर माह में स्वामी जी मलेरिया से बीमार हो गये। गुरुदेव ने इन्हें स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी के साथ एक धर्मनिष्ठ चिकित्सक श्री बी. ए. वैद्य की देख-रेख में पूर्ण उपचार तथा विश्राम के लिए नागपुर भेज दिया। उनका धनतोन्नी में अपना चिकित्सालय था तथा वह नागपुर के मेयो चिकित्सालय में एक अवैतनिक चिकित्सक थे। स्वामी जी ने यहीं पर चिकित्सालय के रेडियो में गान्धी जी की हत्या का उद्वेगकारी समाचार सुना । यद्यपि वह वहाँ एक रोगी थे, तथापि उनसे उस महान् आत्मा के निधन पर एक प्रार्थना-सभा का संचालन करने तथा अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए अनुरोध किया गया।
स्वामी जी स्वास्थ्य-लाभ के पश्चात् आश्रम वापस आ गये। उस समय स्वामी निजबोध जी, जो सन् १९४४ से दिव्य जीवन संघ के महासचिव रहे थे, इस बोझिल कार्य से अवकाश ग्रहण करना चाहते थे। गुरुदेव ने अब चिदानन्द से इस पद का भार लेने के लिए कहा जिसे स्वामी जी को पन्दरह वर्ष की दीर्घावधि, १९६३ तक सँभालना पड़ा।
जो भी हो, स्वामी जी साधकों की अथक टोली के अनभिषिक्त अग्रणी थे ही। अब गुरुदेव ने इसको विधिवत् मान्यता दे दी। किन्तु इस मान्यता का अर्थ इनके दैनिक कर्तव्यों में और अधिक वृद्धि भी थी। इनका मानसिक सन्तुलन निश्चय ही विलक्षण था। तभी वह इतने अधिक वर्षों तक प्रतिदिन इतने अधिक कार्यों की ओर ध्यान दे सके। यद्यपि वह एक अन्ताराष्ट्रीय संस्था के महासचिव के प्रतिष्ठित पद पर थे, किन्तु वह कभी भी क्षणमात्र को न तो उल्लसित हुए और न दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ही किये। वह जो वस्त्र धारण करते थे वह घुटनों से नीचे तक नहीं पहुँचता था। गुरुदेव ने एक बार विनोद में इनसे कहा : "ओ जी! आप दिव्य जीवन संघ के महासचिव हैं। आप सुन्दर लम्बे वस्त्र क्यों नहीं धारण करते?" स्वामी जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि पहाड़ियों पर चपल गति से चलने के लिए मैं छोटी तौलियों को पहनना अधिक पसन्द करता हूँ। वस्तुतः स्वामी जी अपने स्वास्थ्य की सर्वथा उपेक्षा कर कार्य-बाहुल्य में इतना तल्लीन रहते थे कि ऐसे व्यस्त समयों में गुरुदेव सूचना लगवा दिया करते थे : "प्रत्येक दर्शक स्वामी चिदानन्द से प्रातः ९ तथा १० बजे के मध्य केवल पाँच मिनट तक मिल सकता है।"
उनतालीसवाँ जन्मदिवस
गुरुदेव अपने परम प्रिय शिष्य का जन्मदिवस प्रतिवर्ष मनाना आरम्भ कर दिये; किन्तु वह स्वामी जी के वास्तविक जन्मदिवस २४ सितम्बर को न मना कर २४ जून को मनाते थे। क्योंकि आश्रमवासी उनका जन्मदिवस प्रतिवर्ष ८ सितम्बर को मनाते थे, अतः उसके कुछ ही दिनों पश्चात् चिदानन्द का जन्मदिवस मना कर वह उसके महत्त्व को कम नहीं करना चाहते थे। अतएव उन्होंने अनेक वर्षों तक चिदानन्द जयन्ती जून माह में मनायी। गुरुदेव के आदेश से स्वामी चिदानन्द का उनतालीसवाँ जन्मदिवस विशेष रूप से भव्य उत्सवोचित आमोद-प्रमोद तथा अत्यधिक गौरवपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर गुरुदेव ने घोषणा की : "स्वामी चिदानन्द जी का जन्म-दिवस मनाना वास्तव में भगवदाराधन है।" उन्होंने स्वामी जी के पराविद्या के ज्ञान की उपलब्धि को मान्यता दी तथा उन्हें 'अध्यात्म-ज्ञान-ज्योति' की पवित्र उपाधि से सम्मानित किया। भक्तों तथा जिज्ञासुओं ने स्वामी जी का मूर्तिमान् भगवान् के रूप में अभिनन्दन किया। अपने अभिनन्दन के उत्तर में उन्होंने कहा कि वह उनकी सभी सकामनाओं तथा विचारों को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात् उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह सब गुरु-कृपा ही है। उन्होंने अपनी तुलना एक मूर्तिकला-कृति से की और कहा कि यदि मूर्ति में कहीं पर कुछ भी सौन्दर्य है तो उसका श्रेय मूर्तिकार को ही जाना चाहिए। उन्होंने उपसंहार करते हुए कहा : "स्वामी चिदानन्द के दिव्य यन्त्रकार स्वामी शिवानन्द हैं।" यह जानना रोचक होगा कि इस पवित्र अवसर पर स्वामी चिदानन्द के गुरुभाइयों ने प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक उनके चरणों का दुग्ध तथा गंगाजल से अभिषेक कर, पुष्प अर्पण कर कर्पूर से नीराजन कर उनकी पादपूजा की मानो कि वे गुरुदेव के ही पावन चरण हों।
एकान्त जीवन
इसके बाद से चिदानन्द पूर्ण एकान्त तथा एकमात्र ध्यान का जीवन-यापन करने को लालायित रहते थे। गुरुदेव उनकी मनोदशा को समझ गये तथा उन्होंने उन्हें बदरीनारायण के विविक्त स्थान में जाने के लिए परामर्श दिया जिससे वह वहाँ बिना किसी भी चित्तविक्षेप के सर्वोच्च कोटि की साधना चालू रख सकें। इस भाँति स्वामी जी ने अक्तूबर १९५६ के प्रारम्भ के दश दिनों तक बदरीनाथ धाम के परम पवित्र स्थान में प्रगाढ़ ध्यान में अपने को संलग्न रखा। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान में नर-नारायण चिरन्तन तप कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तपश्चर्या को सम्पूर्ण मानव-जाति के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।
एकान्त तथा आभ्यन्तर ध्यान की अल्पावधि के बाद ही सक्रिय सेवा की अवधि आयी। स्वामी जी गुरुदेव की आज्ञा के पालनार्थ हिमालय के शिखर से त्वरित गति से नीचे आ गये। गुरुदेव ने कोलकाता में १९ अक्तूबर से २२ अक्तूबर तक के लिए नियत 'आठवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन' की अध्यक्षता करने के लिए उन्हें प्रतिनियुक्त करने का निश्चय किया था। नीचे आते समय मार्ग में उन्हें मूसलाधार वर्षा का सामना करना पड़ा। पुल टूट गये थे तथा सड़कें संकटपूर्ण थीं। प्रत्येक प्रतिकूलता तथा असुविधा का सामना करते हुए तथा वर्षा-जल से पूर्णतया सराबोर उन्होंने अपनी स्थिर गति को बनाये रखा और गुरुदेव के पास ठीक उस दिन वापस आ गये जिस दिन के लिए उन्होंने गुरुदेव को वचन दिया था।'[6]
स्वामी जी सम्मेलन की, जिसका विधिवत् उद्घाटन डा. कालिदास ने किया था, अध्यक्षता करने के लिए ठीक समय से कोलकाता पहुँच गये। हाल में प्राप्त अपने आध्यात्मिक ओज की पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने जनसमूह पर अमिट प्रभाव छोड़ा। स्वामी जी ने पाटन में 'नवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन' की अध्यक्षता करने के लिए गुजरात को प्रस्थान किया। कोलकाता की भाँति यहाँ भी उन्होंने अपनी असाधारण सौजन्यता तथा आध्यात्मिक शक्ति से श्रोताओं को अभिभूत कर लिया।
इस अल्पकालिक स्फूर्तिकारी तथा सक्रिय सेवा के अनन्तर स्वामी जी की आन्तर सत्ता एक बार पुनः मौन तथा एकान्तवास की ओर प्रभावशाली रूप से आकृष्ट हुई। उन्होंने गुरुदेव से हिमालय में किसी उत्तुंग निर्जन शैल पर चले जाने तथा प्रभु के साथ आनन्दमय अवस्था में पूर्णत: निमग्न रहने की अनुमति माँगी, किन्तु वह आश्रम के अत्यावश्यक कार्यों से अपने को मुक्त न कर सके और दीर्घकालिक तपश्चर्या की योजना ले कर बदरीनाथ धाम की द्वितीय यात्रा सन् १९५८ के ग्रीष्मकाल में ही कर पाये। इस बार वह पैदल गये और पहाड़ियों पर अत्यधिक शारीरिक आयास से आरोहण किया। रात्रि को वह मेषपालों की झोपड़ियों में आश्रय लेते तथा भेड़ों से परिवृत्त उनके पुआल-निर्मित बिछौनों पर शयन किया करते थे। यात्रा की इन समस्त कठिनाइयों के मध्य भी उन्होंने असाधारण शान्ति तथा आनन्द का बोध अनुभव किया। मार्ग में वह एक स्थान पर एक शिवालय में रुके जहाँ शिवलिंग हिम से आच्छादित था। उस प्रशान्त तथा विरल शिखर पर प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई न था। वह उस एकान्त के परमानन्द में अपने को जिज्ञासु के प्रति उद्घाटित कर रहे थे। स्वामी विवेकानन्द ने भी अमरनाथ में अपने परिव्राजक-काल में इसी प्रकार की अनुभूति की थी। बदरीनाथ पहुँच कर उन्होंने अलकनन्दा में स्नान किया तथा सुदीर्घकाल तक आनन्दमय अवस्था में अपने को योग में दृढ़तापूर्वक स्थित रखा।
पश्चिमी गोलार्ध में
यह पुनः भगवदिच्छा ही जो लोकसंग्रहार्थ उन्हें नीचे लायी जब कि वह निर्विकल्प-समाधि में स्थायी रूप से प्रवेश कर जाने तथा अपने भौतिक शरीर को त्याग देने के लिए उत्कण्ठित थे। गुरुदेव शिवानन्द के सत्संकल्प के माध्यम से अभिव्यक्त भगवदिच्छा मानव-जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए उन्हें पार्थिव धरातल पर नीचे लायी। स्वामी जी भगवान् के आदेश के पालनार्थ दिसम्बर १९५८ में हिमालय की विरल ऊँचाई से नीचे उतरे तथा गुरुदेव से मिले। गुरुदेव उन्हें विरल दिव्य प्रभा से दीप्तिमान देख कर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनकी इच्छा थी कि ऐसी देदीप्यमान आत्मा पाश्चात्य जगत् के साधकों को प्रबुद्ध करने के लिए उनके धर्मदूत के रूप में आगे जाये जब कि स्वामी जी एक बार पुनः आन्तर ध्यान में निमग्न होने के लिए उत्तरकाशी जाने को लालायित हो रहे थे, परन्तु अमरीका के भक्तों के साग्रह अनुरोध पर गुरुदेव ने स्वामी जी को नयी दुनिया (अमरीका) के लोगों के लिए योग तथा वेदान्त का सन्देश ले कर वहाँ जाने के लिए कहा। और इस भाँति अपने गुरुदेव की इच्छाओं के पालन के लिए उन्होंने हिमालय के प्रशान्त तथा शुद्ध निवास स्थान से अमरीका के हलचलपूर्ण, अशान्त राजधानीय नगरों की ओर प्रस्थान किया। पाश्चात्य गोलार्ध में स्वामी जी की यात्राएँ मध्य यूरोप से इंग्लैंड तक, उत्तरी अमरीका से दक्षिणी अमरीका तक विस्तृत थीं। जहाँ-कहीं भी वह गये, उनका आगमन एक बहुत ही अद्वितीय तथा मांगलिक घटना के रूप में घोषित किया गया। उन्होंने नवम्बर १९५९ से दिसम्बर १९६१ तक पाश्चात्य गोलार्ध की यात्रा की तथा अपने जिज्ञासु श्रोताओं के चित्त पर गम्भीर प्रभाव छोड़ा। अमरीकावासियों ने भारत से आने वाले सर्वाधिक उन्नत योगी, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों से अत्यधिक सम्पन्न तथा पाश्चात्य मस्तिष्क का वास्तव में गम्भीर रूपान्तरण सम्पन्न करने में सक्षम व्यक्ति के रूप में उनका स्वागत किया। जिन अगणित घरों, संस्थाओं तथा नगरों में वह गये, वहाँ उन्होंने दिव्य जीवन का सन्देश पहुँचाया तथा शुरू से अन्त तक भारतीय संन्यासी की वृत्ति को प्रयत्नपूर्वक बनाये रखा। जिसे भौतिकवादी पश्चिम के अनेक स्थानों की आध्यात्मिक विजय कहा जा सकता है, उसे प्राप्त कर वह जनवरी १९६२ में अपूर्व सफलता के साथ भारत वापस आये और गुरुदेव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने तुरन्त ही वेगपूर्वत चल पड़े।
अल्पकालिक अज्ञात संचार
स्वामी जी को दो वर्ष तक पाश्चात्य जगत् के कार्य-समाकुल वातावरण में, पूर्ण विकसित कटु रूप की राजसिक गतिशीलता में रहना पड़ा था। उनके ही शब्दों में: “भीड़भाड़, कोलाहल तथा बेचैनी में रहने तथा लगातार वार्तालाप करते रहने के पश्चात् मैं यहाँ शान्ति की लालसा से आया।" नयी दुनिया अमरीका से वापस आने के तुरन्त बाद ही उन्होंने अपने अन्तर में वन तथा अरण्यों के आह्वान की, आन्तरिक नीरवता तथा विश्रान्ति की लालसा की तीव्र वाणी सुनी। अतएव उन्होंने आश्रम-जीवन से दूर रह कर एकाकी परिवाज्रक-जीवन-यापन करने की अनुमति प्रदान करने के लिए गुरुदेव से उत्कट अनुरोध किया। वह एकमात्र पूर्ण एकान्तवास के लिए लालायित थे। वह किसी अज्ञात स्थान में भगवान् में तल्लीन रह कर पूर्णतः अपरिचित रूप से अपना नश्वर शरीर त्याग देना चाहते थे। अपनी अनुमति देना गुरुदेव के लिए सहज न था। यद्यपि गुरुदेव अपने प्रिय शिष्य को पश्चिम में दो वर्ष की दीर्घावधि तक अविरत तथा क्लान्तिकर यात्रा के बाद इतना शीघ्र परिव्राजक का क्लेशकर जीवन अपनाने की अनुमति देना नहीं चाहते थे तथापि स्वामी जी का अनुरोध इतना गम्भीर तथा अवधूत-जीवन के लिए उनका वर्तमान राग इतना प्रबल था कि उन्होंने उसे अस्वीकार करना नहीं चाहा।
स्वामी जी ने अप्रैल १९६२ में दक्षिण भारत की तीर्थयात्रा के लिए आश्रम से प्रस्थान किया। उन्होंने स्वयं बतलाया था कि इस यात्रा का उद्देश्य अपने सूक्ष्म मन पर पड़े हुए पाश्चात्य रंग से रँगे वातावरण के यत्किंचित् प्रभाव का प्रक्षालन करना था। वह निस्सन्देह सर्वधा पवित्र तथा निष्कलंक थे, किन्तु जैसा कि वह पहले बल दे कर कहा करते थे कि आन्तर शौच की कोई सीमा रेखा नहीं है। भौतिकता-प्रधान वातावरण वाले पाश्चात्य देशों में दीर्घावधि तक निवास करने के पश्चात् उनके अनजाने में उनके मस्तिष्क को जो रजोगुण के कण मात्र ने भी आक्रान्त किया हो, उससे उसे शुद्ध करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से तप की इस अवधि को झेला। उन्होंने उच्चतर मर्यादा के अनुपालन तथा मन की आत्मतुष्टि के विरुद्ध सतर्कता के रूप में कठिनाइयों का जीवन वरण किया और अपने को तप की अग्नि परीक्षा में डाला। यहाँ वह स्वामी कृष्णानन्द के शब्दों में "पवित्र भारतवर्ष की आदर्श संन्यासी-परम्परा में एक सद्वंशज के रूप में उभर कर बाहर आये।"
स्वामी जी ने सभी लोगों से दूर रहने तथा बिना किसी की जानकारी के प्रच्छन्न रूप में देवालयों से विविक्त स्थानों में विचरण करने का निश्चय कर लिया था, किन्तु ठीक उसी समय डा. बी. जी. अध्वर्यु ने साग्रह अनुरोध किया कि वह दिव्य जीवन संघ की राजकोट शाखा में उनकी व्यवस्था में भगवद्गीता पर श्रेणीबद्ध प्रवचन करने की कृपा करें। स्वामी जी ने इस अभिजात आत्मा का अनुरोध कभी भी अस्वीकार नहीं किया था। उन्होंने गुरुदेव को लिखे हुए अपने अनुरोध पत्र को दिखाया। गुरुदेव ने भी अपनी ओर से आग्रह किया कि वह डा. अध्वर्यु को निराश न करें। इन परिस्थितियों में अपनी योजना के अनुसार अज्ञात संचार में छलाँग न लगा कर उन्होंने गुजरात की ओर प्रस्थान किया। गुजरात के तीन सप्ताह के अपने आवास-काल में उन्होंने राजकोट तथा वीरनगर में श्रेणीबद्ध भाषण दिया। अपने एक पुराने वायदे को पूरा करने के लिए वह वीरनगर से मुम्बई गये। जब वह कैलीफोर्निया में थे तब उन्होंने मुम्बई के एक उत्कट भक्त को एक बार उसके यहाँ ठहरने का वचन दिया था। उस पुराने वायदे के अनुसार वह उस भक्त के पास दो-चार दिन ठहरे।
तदनन्तर वह 'गेट वे आफ इण्डिया' (भारत का प्रवेश-द्वार) से एक एकाकी तीर्थयात्री के रूप में निकल पड़े। अब वह एक सर्वथा अपरिचित परिव्राजक संन्यासी थे। आश्रम में कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता था कि वह कहाँ गये। देश के किसी भक्त को उनके पते-ठिकाने के विषय में कोई जानकारी न थी। स्वर्गिक आनन्द से देदीप्यमान तथा सदा दिव्य चेतना में निमज्जित वह पुण्यमयी भारत भूमि में स्वच्छन्द तथा अक्षुब्ध भ्रमण करते थे। जो कुछ भी दैनिक भिक्षा के रूप में प्राप्त हो जाता, उससे ही सन्तुष्ट रह कर वह परम सादगी तथा स्वैच्छिक कठिनाई का जीवन-यापन करते तथा चाहे चल रहे हों अथवा विश्राम कर रहे हों, सदा अन्तरस्थ आनन्द की अवस्था में संस्थित रहते थे। यदि स्वामी जी ने स्वयं कृपा न की होती तो कदाचित् उनका अज्ञात संचार सर्वथा अज्ञात ही रह जाता। लेखक के इस विनम्र प्रार्थनामय आग्रह पर कि उनके यात्रा-वृत्तान्त की जानकारी परिव्राजक जीवन के अभिलाषी सभी जिज्ञासुओं के लिए लाभकारी होगी, उन्होंने लेखक को अपनी यात्रा के प्रमुख भाग को कृपापूर्वक संक्षेप में बतलाया। निस्सन्देह उस भाग्य-निर्णायक वर्ष में स्वामी जी के सभी अनुभवों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानना अथवा वर्णन करना सम्भव न होगा। उसका केवल स्थूल सामान्य चित्र ही अंकित किया जा सकता है।
स्वामी जी ने सर्वप्रथम कुछ दिन महाराष्ट्र राज्य में व्यतीत किये और तत्पश्चात् वह बेंगुलूरु गये। कर्णाटक राज्य में वह पवित्र मन्दिरों में गये तथा वहाँ उन्होंने उन पवित्र स्थानों में अर्चावतार के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान् प्रभु से प्रार्थनाएँ कीं। मैसूर तथा मरकारा से हो कर उन्होंने भगवती माँ चामुण्डेश्वरी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और तब वह अपने प्रिय गुरुभाई स्वामी कृष्णानन्द के जन्म-स्थान पुत्तूर पहुँचे। तत्पश्चात् वह अपने जन्म-स्थान मंगुलूरु सम्भवतः माता सरोजिनी की पावन स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने गये। तत्पश्चात् उन्होंने वेदान्त-दर्शन के द्वैतवाद के प्रतिपादक मध्वाचार्य के जन्म-स्थान महाविष्णु-क्षेत्र उड़िपी को स्थानान्तर किया। उड़िपी पुरन्दरदास के जन्म-स्थान के रूप में भी प्रख्यात है। पुरन्दरदास प्रसिद्ध दास-परम्परा के प्रवर्तक थे जिसमें जीवात्मा परमात्मा का नित्य दास माना जाता है। भगवान् कृष्ण को अपनी प्रार्थना निवेदन कर तथा मध्वाचार्य और भक्त पुरन्दरदास के पुण्यकार्यों को स्मरण कर उन्हें यहाँ आनन्दमय अनुभव हुआ। उड़िपी से वह प्रख्यात देवीक्षेत्र कोल्लूर गये वहाँ भगवती लक्ष्मी माता की मूकाम्बिका के रूप में पूजा की जाती है। कल्याणी माँ अन्नपूर्णेश्वरी मूक भक्तों तक की कामना पूर्ण करने के लिए प्रख्यात हैं और इस स्थिति में वह मूकाम्बिका नाम से ज्ञात हैं। स्वामी जी मानव-जाति के सभी अभावग्रस्तों, रोगियों तथा परित्यक्त लोगों की समृद्धि तथा उत्थान हेतु प्रार्थना करने के लिए यहाँ कुछ समय रुके और तत्पश्चात् कांजनगढ़ की ओर आगे बढ़े। यहाँ आनन्दाश्रम में उन्होंने अपने प्रिय पापा परम पावन श्री स्वामी रामदास के पावन चरणों में श्रद्धामय प्रणाम किया जिनकी पुस्तक 'भगवान् की खोज में' ने उनमें जीवन के उषाकाल से ही आध्यात्मिकता का बीज वपन किया था। उन्होंने वहाँ श्रद्धेय पापा की प्रमुख शिष्या महाभाग माता कृष्णाबाई के भी दर्शन किये। कांजनगढ़ से वह कण्णूर गये और तत्पश्चात् एक बार पुनः उड़िपी वापस आ गये। संयोगवश एक साधु ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें अपने आश्रम में आने के लिए विवश किया। स्वामी जी वहाँ से चेन्नै गये और फिर वहाँ से भगवान् वेंकटेश्वर के पवित्र धाम तिरुपति गये। भगवान् तिरुपति बाला जी को प्रार्थना निवेदन कर उन्होंने श्री रमण महर्षि की तपोभूमि अरुणाचलम् की यात्रा की। यहाँ स्वामी जी ने भगवान् रमण को उनके पवित्र समाधि-मन्दिर में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा कुछ समय के लिए आन्तर नीरवता में प्रवेश कर गये।
स्वामी जी की पवित्र तीर्थयात्रा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष भी था। उन्होंने अपने परिव्राजक जीवन-काल में निर्धनों तथा रोगियों की सहायता करने का कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दिया। बस से यात्रा करते समय उन्होंने तिरुकोयलूर के निकट एक वृद्धा महिला को देखा जो निस्सहाय तथा अन्धी थी। वह तुरन्त बस से नीचे उतर आये तथा उन्होंने उसकी कठिनाई के सम्बन्ध में उससे पूछताछ की। वह एक रोमन कैथोलिक पुजारी तथा पुलिस के कुछ कर्मचारियों से मिले और उस स्थान से जाने से पूर्व उस बेचारी महिला के लिए आवश्यक सहायता का निश्चित प्रबन्ध कर दिया।[7] वह जब इस प्रकार सेवा कार्यों में संलग्न होते तो किसी भी व्यक्ति के लिए यह अनुमान करना कठिन होता कि वह हिमालय के एक परिव्राजक स्वामी हैं। अनुकम्पा के इस प्रकार के कार्य उनके व्यक्तित्व के सद्गुणों का एक सर्वाधिक देदीप्यमान चिह्न रहा है। चाहे वह नयी दुनिया अमरीका में हों अथवा शिवानन्दाश्रम के काम में संलग्न हों, अथवा दूर दक्षिण में एकाकी तीर्थयात्री के रूप में अज्ञात रूप से भ्रमण कर रहे हों, उन्होंने निर्धनों तथा रोगियों में अन्तस्थित स्थित भगवान् की सेवा करने के किसी भी अवसर की उपेक्षा नहीं की।
अब हम तीर्थयात्रा के वृत्तान्त पर वापस आते हैं। स्वामी जी अब चित्तूर जिले के तिरुत्तणि स्थान पर प्रख्यात सुब्रह्मण्य-क्षेत्र गये जो कार्तिकेय की पूजा से सम्बन्धित छह धार्मिक महाकेन्द्रों में से एक है। यहाँ उन्होंने रमणीय पहाड़ी के निभृत स्थान में भगवान् कार्तिकेय को अपनी प्रार्थना निवेदित कर चिदम्बरम् की यात्रा की जो चेन्नै से एक सौ पचास मील तथा दक्षिण आरकाट जिले के समुद्रतट से सात मील दूर है। चिदम्बरम् में भगवान् नटराज की पूजा करने के पश्चात् उन्होंने श्री मुशनम् में वराह अवतार के दुर्लभ मन्दिर का दर्शन किया। तत्पश्चात् उन्होंने कुम्भकोणम् की यात्रा की जो अपने बहुसंख्यक प्राचीन मन्दिरों के लिए प्रख्यात है। यह दक्षिणी रेलवे के मुख्य रेल मार्ग पर एक रेलवे स्टेशन है तथा तंजावूरु जिले में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कुम्भकोणम् में उन्होंने सारंगपाणि-मन्दिर, रामस्वामी-मन्दिर तथा कुम्भेश्वर मन्दिर में भगवान् की पूजा की। वह कुम्भकोणम् के निकट स्वामीमलय में स्वामीनाथ के नाम से अभिहित भगवान् कार्तिकेय को समर्पित प्रख्यात मन्दिर में भी गये। मवूर में आर. एस. शर्मा नामक एक उत्कट तमिल भक्त द्वारा कोलकाता के निकट दक्षिणेश्वर की भवतारिणी देवी के मन्दिर के नमूने पर निर्मित एक विशेष असार्वजनिक मन्दिर में काली देवी के दर्शन कर वह सुखी हुए। तत्पश्चात् स्वामी जी वडलूर गये जहाँ वह सन्त रामलिंग स्वामी के प्रसिद्ध समाधि-मन्दिर में प्रार्थना तथा ध्यान में लीन हो दीर्घ काल कर बैठे रहे।[8]
वडलूर से वह चेंगलपट के कांजीवरम् (कांची) गये। वहाँ उन्होंने भगवान् वरदराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा श्री शंकराचार्य का प्रसिद्ध मठ भी देखा। तत्पश्चात् चेन्नै तथा कोयम्बतूर में अल्पकालिक आवास के अनन्तर वह पलनि के उन्नत पर्वत पर स्थित अतीव प्रख्यात कार्तिकेय क्षेत्र गये तथा वहाँ पर उन्होंने दण्डपाणि के नाम से प्रसिद्ध भगवान् कार्तिकेय को अपनी प्रार्थना निवेदन की। यहाँ भगवान् दण्डपाणि शक्तियों से वियुक्त अपने हाथ में शूल धारण किये हुए अकेले खड़े हैं। स्वामी जी ने पलनि से बस द्वारा मदुरै की यात्रा की जहाँ उन्होंने भगवती माँ मीनाक्षी देवी की पूजा की। तदनन्तर वह पत्तमडै गये जहाँ की पवित्र भूमि में गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज अवतरित हुए थे। स्वामी जी वहाँ श्रद्धापूर्वक बैठ गये तथा गम्भीर ध्यान में उन्होंने महान् गुरुदेव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहाँ ही उनको यह सत्संकल्प हुआ कि श्री गुरुदेव की स्मृति को उनके जन्म-स्थान में स्थायी बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। एक समय आया जब उनके सत्संकल्प ने मूर्त रूप लिया और आज इस जगद्गुरु के आगमन का स्मरणोत्सव मनाने के लिए वहाँ एक मन्दिर अवस्थित है।'[9]
स्वामी जी पत्तमडै से तेनकाशी गये और वहाँ जलप्रपात की मनोरम भूमि में आत्मविस्मृत हो गये। तत्पश्चात् वह स्वामी विवेकानन्द के नाम पर विश्रुत कन्याकुमारी गये जहाँ उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के प्रेरणादायी जीवन तथा सन्देश के चिन्तन में कुछ समय व्यतीत किया। स्वामी विवेकानन्द के प्रति उनमें इतनी श्रद्धा है कि वह अपने इन सब दुर्वह कर्तव्यों के होते हुए आज भी बुलाये जाने पर कन्याकुमारी, दिल्ली तथा अन्य स्थानों के विवेकानन्द-केन्द्रों के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए अपना कुछ समय देते हैं।
कन्याकुमारी से स्वामी जी ने तिरुचेन्दूर की यात्रा की जो तिरुनेल्वेलि जिले की सुदूर सीमा के समुद्र तट पर एक अन्य प्रसिद्ध कार्तिकेय क्षेत्र है। इस मन्दिर में भगवान स्कन्द को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर वह 'रामेश्वरम्' गये जो भारतवर्ष के चार बड़े धामों में से एक है। यहाँ उन्होंने भगवान् शिव का पूजन किया। तत्पश्चात् वह त्रिची तथा तंजावूरु गये। वहाँ से वह परम पावन श्री राघवेन्द्र स्वामी की पुण्यस्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रायचूर के निकट मन्त्रालय गये। मन्त्रालय में वह लगभग एक मासार्ध रहे। कहा जाता है कि अपनी महासमाधि से ठीक कुछ समय पूर्व राघवेन्द्र स्वामी ने घोषित किया था: "मैं इस स्थान से आगामी सात सौ वर्षों तक कार्य करता रहूँगा।" पाठकों को स्मरण होगा कि स्वामी जी के पिता श्रीनिवास राव जी ने एक बार अपना गृह त्याग कर सूक्ष्म शरीरधारी राघवेन्द्र स्वामी के आध्यात्मिक संरक्षण में इस पवित्र स्थान में कुछ समय व्यतीत किया था। स्वामी जी यहाँ पर नित्यप्रति पावनी तुंगभद्रा नदी में स्नान करने तथा गम्भीर चिन्तन तथा ध्यान में विलीन होने से अत्यधिक आनन्दित थे।
मन्त्रालय से उन्होंने पण्ढरपुर की यात्रा की जहाँ विठ्ठल-रूप में भगवान् विष्णु महाराष्ट्र के प्रमुख देवता के रूप में सुशोभित हैं। यहाँ स्वामी जी ने नामदेव, तुकाराम, एकनाथ तथा ज्ञानेश्वर जैसे महान् भक्तों की जीवनियों तथा उनके कार्यों का अध्ययन तथा चिन्तन करते तथा प्राचीन काल के उन यशस्वी सन्तों के साथ अपने में एक प्रकार की आध्यात्मिक समानुभूति का विकास करते हुए तीन माह व्यतीत किये। वह प्रतिदिन कुछ समय तुकाराम के अभंगों तथा अन्य सन्तों द्वारा रचित स्तोत्रों से भगवान् की स्तुति करने में व्यतीत करते थे।
इस प्रकार दक्षिण में व्यापक रूप से भ्रमण कर लेने पर, स्वामी जी अब गम्भीर साधना के लिए एक स्थान में कुछ समय के लिए टिक जाना चाहते थे। इसलिए वह केन्द्रीय रेलवे के मुम्बई-चेन्नै रेल मार्ग पर शोलापुर के कुछ मील दक्षिण में स्थित गाणगापूर गये। वास्तविक गाणगापूर-क्षेत्र रेलवे स्टेशन से दक्षिण की ओर कोई चौदह मील पर होगा। दत्तात्रेय इस तीर्थ के अधिष्ठाता देवता हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि नृसिंह सरस्वती ने, जो दत्तात्रेय के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, इस पवित्र क्षेत्र में अपने सदा उपस्थित रहने का आशीर्वाद दे रखा है। स्वामी जी ने इस पवित्र भूमि में ठहरने तथा उग्र तप और ध्यान करने का अन्तिम निर्णय ले लिया।
अपने लम्बे यात्रा-काल में जब वह भूमि पर शयन तथा भिक्षा पर निर्वाह करते हुए परिव्रजन कर रहे थे, उस समय वह अन्तर में तप की अग्नि से प्रज्वलित थे, देदीप्यमान थे। अब उन्होंने गाणगापूर में एक साधारण पर्णकुटीर में एक यति के रूप में रहने तथा तप की अग्नि को सम्पोषित कर अनिर्वाप्य तथा शाश्वत ज्वाला बनाने का निश्चय किया। अक्तूबर १९६२ से मई १९६३ के इन आठ लम्बे महीनों तक प्रतिदिन भिक्षा के रूप में प्राप्त दले हुए मोटे अन्न पर उन्होंने निर्वाह किया। यह एक रोचक संयोग था कि उसी क्षेत्र को एक अन्य महान् योगी ने पवित्र किया था। उनका नाम भी चिदानन्दू था।'[10]
स्वामी जी ने इस पवित्र स्थान में उग्र, अबाध तथा दीर्घकालीन ध्यान के लिए अपने को विधिवत् अर्पित कर दिया। उनकी सम्पूर्ण सत्ता दिन-प्रति-दिन नित्य गम्भीर होते जा रहे ब्रह्मविचार के जल में निमज्जित रहती। नामरूपमय जगत् विलीन हो गया और बहुत ही सहज तथा स्वाभाविक रूप से वह अपने निज-स्वरूप में स्थित हो गये। यह कदाचित् उनके जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समय था। सम्पोषण का उनके पास कोई निश्चित साधन न था। वह अनिकेत थे। केवल एक सादा तथा छोटा-सा काषाय वस्त्र उनके शरीर पर लटक रहा था। लोग जो कुछ भी स्वेच्छा से उन्हें प्रदान करते, वही उनके जीवन-निर्वाह का साधन था। भौतिक शरीर उनके लिए मानो कुछ भी न था। वह सदा ही परमोच्चावस्था की चेतना में एकाकी रहते थे। यदि वह अपने अविकल भौतिक शरीर के साथ जीवित रहे तो यह पूर्णतः विश्वयोजना के ही कारण था। वह उच्चतम आत्मत्याग तथा पूर्ण अनात्मशंसा की अवस्था से गुजर चुके थे। उनके लिए कुछ भी करणीय शेष न था। अतः सर्वशक्तिमान् प्रभु की उनके सम्बन्ध में जो-कुछ भी योजना रही हो, उसे मूर्त रूप देना अब उसका ही काम था।
स्वामी जी मई १९६३ में अकस्मात् अस्वस्थ हो गये। जब वह अपने जड़ व्यक्तित्व को तप की अग्नि में पूर्णतः झुलसा देने को तैयार थे, उस समय दैवी योजना द्वारा उसके प्रति प्रखर रूप से सचेत होने को विवश होना पड़ा। भगवान् के रहस्यमय हाथों ने उन्हें गाणगापूर के प्रशान्त वातावरण से मुम्बई में ला फेंका। यहाँ वह अपने वरिष्ठ गुरुभाई श्री स्वामी परमानन्द जी से मिले। वहीं उनकी आवश्यक भैषजिक चिकित्सा की गयी। चिकित्सकों ने उन्हें यात्रा की और अधिक कठिनाई को झेलना छोड़ देने के लिए प्रेरित किया; किन्तु स्वामी जी की और कोई इच्छा नहीं थी। अल्पकालीन उपचार के अनन्तर मुम्बई से प्रस्थान कर वह उत्तर दिशा की ओर हिमालय के केदारनाथ-मन्दिर के मार्ग में पड़ने वाले पर्वतीय स्थान देहरादून को सीधे चल पड़े। वह भगवान् मुरलीधर को अपनी प्रार्थना निवेदन करने के लिए मार्ग में मथुरा तथा वृन्दावन में थोड़ी देर रुके। ऋषिकेश से कतराते हुए देहरादून की ओर आगे बढ़े तथा त्वरित गति से मसूरी के निकट बारलोगंज ग्राम जा पहुँचे। यह समुद्र तट से लगभग ५००० फीट की ऊँचाई पर एक शीत स्थान है। यहाँ रहते हुए तीन दिन व्यतीत हो गये। यहाँ जब वह विश्राम कर रहे थे तथा हिमालय के किसी उच्चतर क्षेत्र की, जहाँ की उन्होंने अभी तक पदयात्रा न की हो, अपनी यात्रा के अन्तिम चरण के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने गुरुदेव से एक रहस्यमय अव्याख्येय खिंचाव अनुभव किया। हिमालय के किसी एकान्त कोने में सदा के लिए चले जाने से पूर्व अपने गुरुदेव के केवल एक बार दर्शन करने की कामना ने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया। उनके अपने शब्दों में : "चौथे दिन मेरे मन में गुरुदेव के केवल एक बार दर्शन करने की अप्रतिरोध्य कामना मुझे अक्षरशः आश्रम में खींच लायी। मैं आश्रम आ गया।" यह दिव्य जीवन संघ के लिए एक निर्णायक महत्त्व की घटना थी।
गुरुदेव के साथ उनके अन्तिम दिनों में
तपश्चर्या तथा अज्ञात संचार की अवधि इस भाँति अकस्मात् समाप्त हो गयी। स्वामी जी २१ जून १९६३ को आश्रम वापस आ गये। गुरुदेव उस समय अपनी महासमाधि की तैयारी कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने कोई विशिष्ट घोषणा नहीं की थी, उन्होंने १४ जुलाई की तिथि की ओर अपने शिष्यों का ध्यान स्पष्ट रूप से आकृष्ट किया था तथा उसे तिथि-पत्र में रेखांकित कर दिया था। उन्होंने उनसे प्रतीयमानतः विनोद के रूप में कहा था कि उन्हें ऊपर ले जाने के लिए वैकुण्ठ से विमान उतर रहा है। उनके अतिरिक्त अन्य किसी को भी इस अनागत का ज्ञान न हो सका कि उनका तिरोभावदिवस इतना शीघ्र आने वाला है। तथापि वह उत्क्रमण की तैयारी कर रहे थे। अतः उनके उत्तराधिकारी को उस महत्त्वपूर्ण दिवस से पर्याप्त समय पूर्व ही आश्रम को वापस लाना पड़ा। यह दैवकृत योजना थी जिसने स्वामी चिदानन्द को बारलोगंज से अपने पग वापस लेने को विवश किया।
जिन दिनों स्वामी जी आश्रम से बाहर थे, लगभग सैकड़ों मील दूर अपने आन्तरिक कोश में छिपे हुए थे, संयोगवश उन्हीं दिनों योग-समाज, चेन्नै के संस्थापक कवियोगी शुद्धानन्द भारती आश्रम पधारे। गुरुदेव उनके बालपन के सखा थे। उनके साथ अपने वार्ता-काल में उन्होंने गुरुदेव से पूछा, "स्वामी जी! कृपया मुझे वह अनश्वर रिक्थ (वसीयत) बतलाइए जो आप मानव जाति को अपनी पुस्तकों तथा भवनों के अतिरिक्त उत्तरदान करेंगे। क्या यह दिव्य जीवन संघ है अथवा संन्यासियों का वह पुण्यशील समाज है जिसे आपने प्रशिक्षित किया है।'' शिवानन्द कुछ समय तक अन्तर्मुख तथा मौन हो गये और तत्पश्चात् उन्होंने कहा: "निस्सन्देह चिदानन्द। वह जीवित रिक्थ हैं जिसे मेरे पश्चात् दिव्य जीवन संस्था का कार्य चलाने के लिए मैं अपने पीछे छोड़ रहा हूँ।" और तब, मानो कि उन्होंने ब्रह्माण्डीय योजना को अपने मन में पहले ही देख लिया हो, आगे कहा, "वह शीघ्र ही आ रहे हैं।" अनेक अवसरों पर उन्होंने यह संकेत दिया था कि चिदानन्द उनके उत्तराधिकारी हैं। सन् १९५३ में आश्रम में आयोजित विश्व धर्म परिषद् के समय उन्होंने कोलकाता के श्री एन. सी. घोष को ऐसा ही इंगित किया था। स्वामी विमलानन्द ने हमें बताया कि इसी भाँति एक अन्य अवसर पर जब गुरुदेव डायमण्ड जुबिली हाल में कार्यालय का कार्य कर रहे थे, गीता-प्रेस के प्रसिद्ध संस्थापक श्री जयदयाल गोयन्दका ने उनका दर्शन किया तथा उनसे अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के विषय में पूछा। गुरुदेव ने उनके प्रश्न का उत्तर देने के बदले चिदानन्द जी को वहाँ तत्काल आने का सन्देश कहला भेजा। स्वामी जी आये और दूर से ही गुरुदेव को श्रद्धापूर्वक तीन बार दण्डवत् प्रणाम किया और तत्पश्चात् गोयन्दका जी को भी साष्टांग प्रणाम किया। अन्य कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कहा भी नहीं गया; किन्तु सहज शिष्टाचार ने गीता-प्रेस के श्रद्धेय संस्थापक पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। चिदानन्द की मात्र उपस्थिति तथा विनम्र दण्डवत् ने उन्हें एक असाधारण भाव से पूरित कर दिया। उन्हें उनका उत्तर प्राप्त हो गया।
इस चुने हुए उत्तराधिकारी को ठीक समय पर आश्रम वापस आना पड़ा। वह वहाँ २१ जून को पहुँच गये तथा पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि गुरुदेव किंचित् अस्वस्थ हैं तथा विश्राम ले रहे हैं; अतएव वह शान्तिपूर्वक अपने कुटीर को वापस चले गये। अगले दिन प्रातःकाल उन्होंने गुरुदेव के कुटीर में उनके दर्शन किये।
गुरुदेव तथा उनके इस चुने हुए शिष्य का पारस्परिक सम्बन्ध भी विलक्षण प्रकार का था। स्वामी जी श्रुतियों का श्रवण करने के लिए अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप कभी नहीं बैठे। गुरुदेव के समय-समय पर कहे हुए शब्द ही इस समर्पित शिष्य के लिए ब्रह्मसूत्र थे। वह न तो निरन्तर गुरुदेव के साथ रहे थे और न उनके निजी सचिव ही रहे थे। उनकी गम्भीरतम श्रद्धा तथा पूर्ण विनम्रता गुरुदेव के साथ परमावश्यक विषय से अधिक वार्ता करने में उनके मार्ग में बाधक थीं। वह सदा ही श्रद्धापूर्ण दूरी बनाये रखते थे और यदि कभी वह उनसे बातें करते भी थे तो वह कुछ आवश्यक इने-गिने शब्द ही बोलते थे। जब स्वामी जी दिव्य जीवन संघ के महासचिव के उच्च पद पर थे और गुरुदेव के साथ व्यक्तिगत वार्ता करने के लिए अनेक अवसर उन्हें उपलब्ध थे, उस समय भी वह सामान्यतः विनम्र तथा संकोची थे। वह यद्यपि परमोच्च अद्वैत स्थिति से सम्पन्न थे तथापि वह शास्त्राज्ञा का पालन करते तथा सदा ही गुरुदेव से यथोचित दूरी पर रहते थे। गुरुदेव यह जानते थे कि उनका चुना हुआ शिष्य पूर्णतया अपने व्यक्तिगत अधिकार से चमक रहा है; सदा दिव्य चेतना में स्थित है तथा उसे उनके समीप रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
किन्तु अब समय आ गया था। गुरुदेव ने अपने उत्तराधिकारी को अपने पास खींच लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के महान् आवेग से उन्हें अनुप्राणित कर दिया। यही रहस्यमय शक्ति-संचार के नाम से विदित है। वह आध्यात्मिक संसर्ग समाप्त हो गया। शिवानन्द अब चिदानन्द में अन्तर्निविष्ट थे। दो एक बन गये। शिवानन्द अब चिदानन्द और चिदानन्द शिवानन्द-स्वरूप थे।
जहाँ तक स्वामी जी का सम्बन्ध है, चूँकि गुरुदेव के दर्शन करने की उनकी अन्तिम अभिलाषा पूर्ण हो चुकी थी, अतः अन्तिम एकाकीपन के लिए वह केदारनाथ के शिखर पर जाने को उत्सुक थे। उन्होंने गुरुदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की और उनका आशीर्वाद माँगा। गुरुदेव की क्रियाविधि को शान्तिपूर्वक ध्यान से देखने के अतिरिक्त उनके पास कहने को कुछ भी न था।
स्वामी जी साक्षात्कार के पश्चात् गुरुदेव के कुटीर से अन्तर्मुखी वृत्ति के साथ बाहर आये। वह आश्रम से उसी दिन अपने अन्तिम प्रयाण की तैयारी कर रहे थे कि उस दिन भारी वर्षा हुई जिससे विवश हो कर उन्हें आश्रम में एक दिन और भी रहना पड़ा। आगामी दिवस को स्वामी कृष्णानन्द जी उनसे मिले और उनसे एक ऐसे व्यक्ति से कुछ वास-गृह के वैध अधीनीकरण की समस्या सुलझाने के लिए अनुरोध किया जो उसे छोड़ने को अनिच्छुक था। स्वामी जी को एक महासचिव के रूप में सर्वप्रथम इसे सुलझाना था। उन्होंने तुरन्त ही शान्ति तथा व्यवस्था के कार्यभारी अधिकारी की सहायता ली और दूसरों को यह स्पष्ट कर दिया कि सांस्थानिक साधु को भी धर्मनिरपेक्ष देश में अवितथ तथा नियमनिष्ठ होना चाहिए। वह समस्या समाप्त हो गयी और अब ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि उनके लिए अब अन्य कोई बाधा नहीं रही। वह जाने को तैयार थे। अभी जब वह अपने कमरे में ही थे, उन्होंने किसी को द्वार खटखटाते तथा 'ॐ नमो नारायणाय' कहते हुए सुना। उन्होंने द्वार खोला तो वहाँ एक वृद्ध सुपरिचित स्वामी मिले जो डा. देवकी कुट्टी से अपने रोग
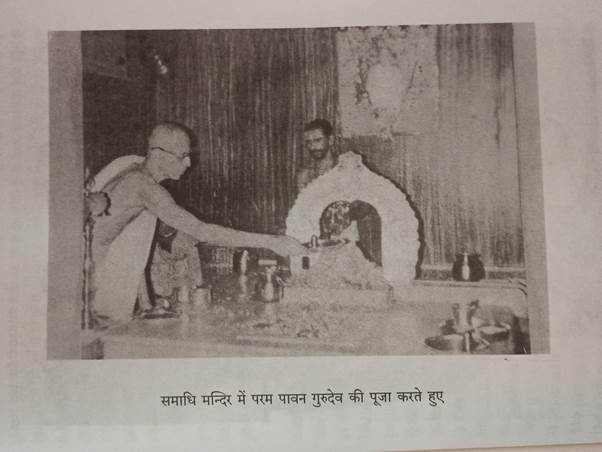
का उपचार कराने की आशा से वहाँ गये थे। स्वामी जी उन्हें तत्काल डा. कुट्टी माता जी के कमरे में ले गये। क्योंकि वह व्यालू कर रही थीं, वह उस रोगी स्वामी के साथ शान्तिपूर्वक बाहर प्रतीक्षा करते रहे। जब कुट्टी माता बाहर आयर्थी तो स्वामी जी को बरामदे में खड़ा देख कर आश्चर्य में पड़ गयीं। स्वामी जी ने उस साधु को उनकी देख-भाल में सौंप दिया तथा स्वयं जाने को मुड़े, किन्तु डा. कुट्टी ने उस रोगी की परीक्षा करने तथा आवश्यक औषधि देने तक स्वामी जी से कुछ समय प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। यह कार्य समाप्त होने पर स्वामी जी आश्रम से प्रस्थान करने की अन्तिम तैयारी करने के लिए अपने कुटीर को जाने को उठ ही रहे थे कि उसी समय आश्रम के अनेक वरिष्ठ भक्त तथा गुरुबन्धु वहाँ आ गये तथा मूल अर्थानुसार उन्हें उठा ले गये। उन्होंने स्वामी जी को रात्रि-सत्संग में सम्मिलित होने तथा वहाँ अपने भावपूर्ण भजन गाने तथा प्रेरणादायी प्रवचन करने के लिए सम्मत कर लिया जिसे उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय से नहीं सुना था। स्वामी जी उनसे सरलता से अपना पीछा नहीं छुड़ा सके, अतएव वह नम्रतापूर्वक भजन हाल चले गये।
जब स्वामी जी ने उस रात्रि को श्रुतिमधुर भजनों को गाया तो सत्संग नये स्फुरणों से पूर्ण हो गया। बाद में जब वह प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने डा. देवकी कुट्टी को चिन्तित मनोदशा में सत्संग से जाते हुए देखा। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो उन्होंने कुट्टी माता जी को पुनः अपने सम्मुख अंजलि बद्ध खड़ी हुई देखा तथा गम्भीर दुःख के साथ यह कहते हुए सुना : "स्वामी जी! आप नहीं जा सकते। गुरुदेव को रक्ताघात हुआ है।" इन शब्दों ने स्वामी जी को स्तम्भित कर दिया। उन्हें ऐसा धक्का लगा कि वह कुछ कह न सके। स्वामी जी ने, जिनकी पूर्ण एकाकी आत्मचिन्तन के अतिरिक्त अन्य कोई भी आकांक्षा नहीं थी तथा जिन्होंने आश्रम से सदा के लिए विदा लेने तथा हिमालय के किसी अज्ञात स्थान में यति का जीवन-यापन करने का निश्चय कर लिया था, तत्काल एक सच्चे शिष्य के रूप में प्रतिक्रिया की। किसी ने भी उनको अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने यहीं रुके रहने तथा अपने गुरुदेव की यत्किंचित् सेवा करने का निर्णय लिया। इस समय उनके लिए केवल एक ही कर्तव्य था और वह था अपने को अपने गुरुदेव के लिए सदा उपलब्ध बनाये रखना। उन्होंने हिमालय की किसी गुहा में एक एकाकी तपस्वी का जीवन-यापन करने की अपनी मनोभिलाषा को सहज दृढ़ता तथा पूर्ण आत्मत्याग से किनारे रख दिया और तुरन्त एक युवक ब्रह्मचारी के अपने भूतपूर्व कर्तव्य को अपना लिया। उनके लिए तात्कालिक कर्तव्य सदा ही प्रार्थना तथा साधना का श्रेष्ठतम रूप रहा है। हो सकता है कि बाद में वह अपने मूल कार्यक्रम में संलग्न हों, किन्त इस समय का कार्य तो स्पष्ट था। स्वामी जी के ही शब्दों में: "जिस दिन मुझे वापस जाना था उसी दिन गुरुदेव प्राणहर रोग से बीमार पड़े। मैं उन्हें रोग-शय्या पर छोड़ नहीं सकता था। अतः मैंने अपने प्रस्थान के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया और इस पूर्ण विश्वास के साथ रुक गया कि जब वह स्वास्थ्य-लाभ करेंगे तथा निरोग होंगे तब मैं जा सकूँगा। शेष आप जानते ही हैं। इसके स्थान पर, उन्होंने स्वयं जाने का निर्णय लिया और जब चिकित्सकगण सोच ही रहे थे कि वह अब निरोग हो रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उसके चौबीस घण्टे के अन्दर स्थिति में परिवर्तन आया और उनका अन्त आ पहुँचा।"
गुरुदेव के लिए यह परम सन्तोष का विषय था कि उनके अज्ञात में तिरोभाव के समय उनका योग्य शिष्य उनके पास था। अपनी महासमाधि से दो दिन पूर्व एक सायंकाल को गुरुदेव ने चिदानन्द जी की ओर उँगली से संकेत कर डा. कुट्टी से कहा : "वरिष्ठतम शिष्य।" उन्होंने इसे दो बार दोहराया। वह पाँचवें दशक में सूचित कर चुके थे कि राव जी उनके उत्तराधिकारी हैं। महासमाधि की पूर्व सन्ध्या को वरिष्ठतम शिष्य के रूप में चिदानन्द जी का बार-बार उल्लेख कर उन्होंने पूर्वसम्प्रत्यय की पुष्टि की थी। जब गुरुदेव के तिरोभाव की अन्तिम घड़ी द्रुतगति से आ रही थी उनका योग्य उत्तराधिकारी उनके पास पूर्ण गाम्भीर्य के साथ उपनिषद् के महावाक्यों का उच्चारण करते हुए पाया गया। अन्त में जब १४ जुलाई १९६३ की अर्धरात्रि को उनके जीवन का अवसान हुआ तो वह गुरुदेव के कुटीर से बाहर आये और एकत्रित आश्रमवासियों से कहा, "यह एक सुन्दर जीवन था और इसने अनेक जीवनों को सुन्दर आकार दिया।"
जगद्गुरु ने अपना जीवनोद्देश्य पूर्ण कर लिया था। वह परम सत्ता में विलीन हो गये। गुरुदेव द्वारा अपने पीछे छोड़े गये शिष्यों में सबसे वरिष्ठ होने के कारण चिदानन्द ने महासमाधि के समय भगवन्नाम का उच्चारण किया। दो दिन पश्चात् १६ जुलाई १९६३ को अपराह्न में गुरुदेव के पवित्र पार्थिव शरीर को पूर्ण गाम्भीर्य तथा विषाद के साथ पवित्र समाधि-मन्दिर में समाधि दे दी गयी। तत्पश्चात् चिदानन्द जी की वैयक्तिक देख-रेख में षोडशी क्रिया सम्पन्न हुई। गुरुदेव के रुग्णता-काल में तथा बाद में उनकी महासमाधि के अनन्तर चिदानन्द ने ही सभी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं की देखभाल की। एक बूँद भी अश्रुपात किये बिना, वह अत्यन्त गम्भीर तथा अन्तर्मुखी वदन से सभी आवश्यक कार्यों को करने तथा आश्रम के भक्तों के शोकसन्तप्त परिवार को सान्त्वना देने में लगे रहे। शेष समय वह सदा ही मौन, प्रशान्त तथा चिन्तनशील रहते थे।
१४ जुलाई १९६३ से १८ अगस्त १९६३ तक प्रकटतः (पद) रिक्तता की मध्यावधि थी। षोडशी-पूजा के समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए दिव्य जीवन संघ के प्रन्यासियों की एक बैठक हुई। उस समय स्वामी चिदानन्द जी मौन ध्यान में अत्यधिक तल्लीन रह कर सबसे दूर रहा करते थे। संघ के सदस्य चाहते थे कि अनिच्छुक स्वामी चिदानन्द जी महाराज गुरुदेव का स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव के नाम में उन्हें वस्तुतः बलात् उस स्थान में डाला गया। सदा की भाँति ही विनीत तथा अनाटकीय रह कर उन्होंने उस समय अपना विचार प्रकट किया: "एक भार ले लिया गया है। इस वहन करना ही होगा।" वह १८ अगस्त १९६३ को औपचारिक रूप से दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उत्तरदायित्व ग्रहण करने के समय उन्होंने गुरुदेव से एक भावपूर्ण बालसुलभ प्रार्थना की : "गुरुदेव की आत्मा से मेरी एकमात्र प्रार्थना यह है कि वह शुद्ध भाव से मुझे सेवा करने, कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करने तथा योग्य रीति से जीवन-यापन करने में समर्थ करें। वह इस सेवक को नम्रता का गुण और निस्स्वार्थपरता तथा समर्पण की योग्यता प्रदान करने से इनकार न करें।”
दिव्य जीवन संघ के इतिहास में १९४३ से १९६३ तक के दो दशक निस्सन्देह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पुण्यसलिला गंगा के तट पर भागवतीय सत्ता ने अपनी विभूति को दो रूपों-कर्मठ गुरु तथा समर्पित शिष्य-में प्रकट किया। भारतवर्ष की पुण्य भूमि में भागवतीय सत्ता अपने को सद्गुरु के रूप में असंख्य बार प्रकट करती है, किन्तु केवल समर्पित तथा अधिकारी शिष्य दुर्लभ होते हैं। स्वामी चिदानन्द इन दुर्लभतम पुष्पों में से एक है जो गुरुदेव की किरण के स्पर्शमात्र से पुष्पित तथा विश्व को मधुर रूप देने के लिए अपने में सुरभि संचित किये हुए आये। अतः ऐसी आत्मसंयमी तथा समर्पित आत्मा सारे विश्वभर के साधकों को उनके जीवन-पथ में मार्गदर्शन कराने वाले सद्गुरु, वास्तविक मित्र, तत्त्ववेत्ता तथा मार्गदर्शक के रूप में उभर कर आगे आये तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गुरुदेव ने उनसे किसी विशेष रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। स्वामी जी ने गुरुदेव के जीवन से जो एकमात्र रहस्य सीखा, वह था: "अपने को रिक्त बनाओ, मैं तुम्हें सम्पूरित कर दूँगा।" चिदानन्द वास्तव में शरणागति तथा गुरुभक्ति के मूर्तिमान आदर्श हैं जो अपने गुरुदेव से अपृथक्करणीय हैं और मानव को महान् पाठ की शिक्षा देने में प्रवृत्त हैं: "ईश्वर परम गुरु है, विश्व सद्गुरु है। यह विश्व ईश्वर का दृग्गोचर रूप है। अतः विश्व गुरु है और जीवन शिष्यत्व है; अतएव आपको विश्व की सेवा तथा विश्व से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही जीवन-यापन करना चाहिए। यह ही मोक्ष-प्रदायक धर्म है।”
चतुर्थ अध्याय
गुरुदेव के साथ युगान्तरकारी यात्रा
"ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तोमामुपासते ।
-और (कोई-कोई) दूसरे लोग ज्ञान-यज्ञ के द्वारा भी पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं।"
भारत का यह संन्यासी, जो विश्व का त्याग करने को उत्सुक था, विधि के विधान द्वारा धर्म का सन्देश घर-घर पहुँचाने वाला परम कर्मठ यायावर-धर्मोपदेशक बन गया। उन्होंने सम्पूर्ण मानव-जाति तक पुण्य-उपदेश को पहुँचाते हुए एक धर्मशास्ता के रूप में प्रथम बार ही १९६३ के बाद विदेश की यात्रा की हो, यह बात नहीं है। वह १९४९ से ही इस विशाल देश तथा विदेश में गुरुदेव के धर्मदूत के रूप में अविरत क्रियाशील रहे हैं। यदि उनके इस कार्य को आरम्भ करने को प्रकट करने के लिए कोई तिथि निर्दिष्ट करनी है तो व्यक्ति को १९४९ तक पीछे मुड़ना होगा जब गुरुदेव ने उन्हें दिव्य जीवन संघ की बिहार प्रादेशिक शाखा के उद्घाटन समारोह में अपना प्रतिनिधित्व करने को पटना जाने के लिए कहा था। उनकी संवेदनशील मुखाकृति, सम्मोहक मुस्कान, दयार्द्र वाणी, मुख का आभामण्डल तथा तेजस्वी वक्तृता ने बिहार के श्रोताओं को पुलकित कर दिया। उन्होंने इन्हें प्रथम श्रेणी का सन्त पाया। वे इस उदीयमान आध्यात्मिक प्रकाश-पुंज के सम्मुख सहन ही नतमस्तक हो गये। इनका वहाँ ऐसा तात्कालिक तथा सशक्त प्रभाव पड़ा कि इनके आश्रम में वापस आने पर स्वयं गुरुदेव ने इन्हें बधाई दी। गुरुदेव ने इस निरतिशय प्रतिष्ठित तथा परम विनीत शिष्य की परीक्षा की तथा लोक-संग्रह के लिए उसकी प्रतिभा को जाना।
गुरुदेव को स्वयं यात्रा करना अभिमत न था। उन्होंने चौदह वर्ष अथवा इससे अधिक समय की दीर्घावधि के अधिकांश काल में अपने को आनन्द-कुटीर तक ही परिरुद्ध रखा। उनके अनेक भक्त अखिल भारत-यात्रा के लिए उनसे बारम्बार अनुनय करते रहे; किन्तु गुरुदेव ने निर्णय लेने को स्थगित ही रखा। अन्त में १९५० में उन्होंने अपना एकान्तवास समाप्त कर भारतवर्ष के कोने-कोने में प्रभु की सन्तान से मिलने के लिए बाहर जाने का निश्चय कर लिया। इस भाँति जब वह ९ सितम्बर १९५० को आनन्द-कुटीर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी युगान्तरकारी यात्रा के लिए स्वामी चिदानन्द को सन्धान-प्रस्तर के रूप में चुना। स्वामी परमानन्द तथा स्वामी वेंकटेशानन्द जैसे अन्य प्रबल समर्थक इस यात्रा के संघटनात्मक वास्तुकार थे तथा उन्होंने श्रेष्ठता से सेवा की; किन्तु सेवा-यात्रा में शुरू से अन्त तक स्वामी चिदानन्द ने ही गुरुदेव की वास्तविक प्रतिकृति के रूप में कार्य किया। उसके पश्चात् भी उन्होंने इस पुण्य भूमि के कोने-कोने तक दिव्य जीवन का सन्देश पहुँचाते हुए समूचे भारतवर्ष की अनेक बार यात्राएँ की हैं; किन्तु गुरुदेव के साथ तथा उनकी सेवा में सन् १९५० की यह अखिल भारत यात्रा वास्तव में सर्वाधिक स्मरणीय थी। वह गुरुदेव के साथ देश के असंख्य जिज्ञासुओं के सम्मुख न केवल गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में अपितु एक परमोत्कृष्ट कोटि के आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में अपने पूर्ण वैयक्तिक अधिकार के आधार पर उपस्थित हुए। इनसे अपने सरल किन्तु मर्मस्पर्शी व्याख्यानों में वेदान्तिक तथ्यों के स्पष्टीकरण द्वारा गुरुदेव के सम्भाषणों को सम्पूरित करने तथा वैयक्तिक प्रदर्शन द्वारा योगासनों के अभ्यास के लिए जनता को प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाता था। यह दीर्घकाल तक बहुसंख्य श्रोतागणों के साथ इनका प्रथम समागम था; किन्तु अपने गुरु के पास रहने के कारण, भीड़ से चाहे वह गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक रूप से कुछ भी हो, इन्हें एक क्षण भी घबराहट नहीं हुई। वह शिवानन्द मिशन के मूल्यवान् कोहनूर की भाँति चमकते रहे तथा उन्होंने सहस्रों मर्त्य प्राणियों को आध्यात्मिक जीवन के प्रवेश-द्वार की ओर आकर्षित किया। अगाध गुरुभक्ति तथा अन्तःप्रज्ञा से परिपूर्ण वह जहाँ-कहीं भी गये वहाँ के लोगों पर उन्होंने अपना अमिट प्रभाव छोड़ा। इस युगान्तरकारी यात्रा के श्रद्धेय स्वामी परमानन्द जी महापराक्रमी आयोजक थे, स्वामी वेंकटेशानन्द यथार्थ प्रतिवेदक थे, नारायण स्वामी तथा स्वामी पूर्णबोधेन्द्र आडम्बर-रहित सहायक थे तथा स्वामी शाश्वतानन्द गुरुदेव की वस्तुतः छाया अथवा उनके अंगरक्षक थे। स्वामी गोविन्दानन्द तथा स्वामी पुरुषोत्तमानन्द ने गुरुदेव को शारीरिक सुख-सुविधा प्राप्त कराने के लिए बड़ी ही सावधानी से अथक कार्य किया। स्वामी ओंकारानन्द आध्यात्मिक साहित्य वितरण के कार्यभारी थे। स्वामी सत्यानन्द हिन्दी-भाषी श्रोताओं में भाषण देते तथा शिवानन्द-साहित्य के विक्रय में स्वामी दयानन्द की सहायता करते थे। पद्मनाभन ने एक छायाचित्रकार के रूप में अपनी सक्षम सेवा से यात्रा को अमर बना दिया। कुछ अन्य लोगों ने भी एकाधिक रूपों में सहायता की; किन्तु इस युगान्तरकारी यात्रा में स्वामी चिदानन्द का अपना विशिष्ट स्थान था। इस भागवत पुरुष का ऐसा अद्वितीय प्रभाव पड़ा कि स्वयं गुरुदेव ने लोगों को इनकी ओर बारम्बार इंगित कर इन्हें अपने सर्वोत्कृष्ट आदर्श के रूप में स्वीकार करने को प्रोत्साहित किया। गुरुदेव ने जिन आदर्शों का उपदेश दिया है, स्वामी चिदानन्द उन सबके आज भी महत्तम जीवन्त आदर्श बने हुए हैं।
गुरुदेव धुर दक्षिण में रामेश्वरम् के उनके प्रख्यात मन्दिर में भगवान् शिव का अभिषेक करने के लिए गंगोत्तरी से पावनी गंगा का पवित्र जल अपने साथ ले गये थे। फैजाबाद में जिज्ञासुओं की एक सभा को सम्बोधित करते हुए स्वामी चिदानन्द ने इसका उल्लेख किया और इसका आन्तरिक अर्थ बतलाया। उन्होंने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि गुरुदेव रामेश्वरम् में अर्पित करने के लिए गंगा के स्रोत से गंगा-जल ले जा रहे हैं; किन्तु वह प्रतीक रूप में समूचे देश को आप्लावित करने के लिए स्रोत से, अपने आत्मज्ञान से ज्ञान-गंगा का जल लिये जा रहे हैं। गुरुदेव की यह तीर्थयात्रा निश्चय ही भारतवर्ष तथा श्रीलंका के लोगों के लिए निस्सन्देह सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक सेवा थी।


गुरुदेव तथा स्वामी जी दोनों की दृष्टि समान थी। दोनों ही इस महान् राष्ट्र की प्राचीन आध्यात्मिक विद्या छात्रों तक पहुँचाने की अविलम्ब आवश्यकता पर बल देते थे तथा दोनों ने ही इस यात्राभर अन्य कार्यक्रमों के मूल्य पर भी अपने प्रबोधक भाषणों से छात्रों को लाभान्वित किया। फैजाबाद में स्वामी जी ने गुरुदेव के भाषण से पूर्व अपना प्रारम्भिक भाषण दिया। यहाँ सच्चरित्र-निर्माण, ब्रह्मचर्य-पालन तथा इस पुण्य भूमि के भाग्यशाली नागरिक होने के अभिमान के पोषण पर उनके हिन्दी के बोधप्रद भाषण ने आश्चर्यजनक अनुक्रिया उत्पन्न की और लखनऊ तथा फैजाबाद-मण्डल के तत्कालीन आयुक्त श्री एस. एल. घर, आई. सी. एस. ने, जिन्होंने इस सभा की अध्यक्षता की, इस युवक संन्यासी ने जनता पर जो चौंका देने वाला प्रभाव डाला, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस भाँति प्रख्यात वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय में स्वामी जी ने छात्र-समुदाय को प्राचीन भारतीय आदर्शों को आत्मसात् करने की प्रेरणा दी। उनके विचारोत्तेजक भाषण ने प्रवर प्राध्यापकों को भी झकझोर दिया।
पटना में ही भारतवासियों को स्वामी जी के गुरुदेव के भावी उत्तराधिकारी तथा गम्भीर ज्ञान-सम्पन्न एक उन्नत कोटि के सन्त होने का पता चल गया। यहाँ स्थानीय रोटरी क्लब में गुरुदेव ने 'विश्व-बन्धुत्व' पर प्रवचन किया। भाषण के अन्त में, जैसा कि प्रायः होता है, प्रश्न का समय था। ऐसा हुआ कि इस अवसर पर गुरुदेव ने स्वामी जी को अपनी ओर से रोटरी क्लब के सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने का निर्देश दिया। इसके द्वारा उन्होंने स्वामी जी के साथ अपनी पूर्ण एकचित्तता सूचित की। इस सुयोग ने जिज्ञासुओं को यह प्रकट कर दिया कि स्वामी चिदानन्द शुद्ध संक्षेत्र (प्रिज्म) हैं जो पिपासु साधकों के पथ को प्रकाशित करने के लिए गुरुदेव के विचारों को परावर्तित करते हैं। क्लब के आधा दर्जन सदस्य स्वामी जी के सम्मुख विविध विषयों को समाविष्ट करने वाली बहुत ही जटिल, दार्शनिक तथा नैतिक समस्याएँ प्रस्तुत करने के लिए एक-एक कर उठे। स्वामी जी ने उनका ऐसे पक्के ढंग से उत्तर दिया कि व्यक्ति को यह सन्देह हो सकता है कि उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वह वहाँ तैयार हो कर गये थे।'[11] श्रोताओं को यह तथ्य सहसा ज्ञात हो गया कि उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रवेश के बिना सुशिक्षित लोगों के प्रवर वर्ग, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री कमलकान्त वर्मा जैसे प्रतिष्ठित लोगों का समावेश था, के सम्मुख तत्काल ऐसे विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगत आध्यात्मिक स्पष्टीकरण दे पाना एक नवयुवक संन्यासी के लिए सम्भव नहीं है। उनके उत्तरों में अपना ही एक विशिष्ट सौन्दर्य था। वे शास्त्रों के प्रमाण, प्रतिभाशाली मस्तिष्क की गहरी पैठ, विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण तथा दिन-प्रति-दिन के सूक्ष्म निरीक्षण को प्रकट करते थे। बैठक के अन्त में जिज्ञासुओं ने स्वामी जी की जागरूकता, समझ तथा विश्वासोत्पादक शक्ति के प्रति अपने समादर-भाव व्यक्त किये। अनुक्रिया का उत्कृष्ट सार कदाचित् आरक्षी महानिरीक्षक श्री ए. के. सिन्हा की केवल एक टिप्पणी उद्धृत कर प्रस्तुत किया जा सकता है। सभा की समाप्ति पर वह आगे बढ़ कर स्वामी जी तक आये और अपने भावोद्गार व्यक्त करते हुए कहा, "स्वामी जी! मैं आप पर गर्व अनुभव करता हूँ।" इस भाँति इस युवा अख्यात संन्यासी ने अपनी तीस वर्ष की आयु में ऐसे प्रौढ़ तथा विवेकी व्यक्तियों के समूह का प्रेम तथा प्रशंसा प्राप्त की जो सहज ही वीरपूजा के आवेश के वशवर्ती होने वाले नहीं थे।
यात्रा-काल में स्वामी जी कार्यक्रमों को प्रायः अपने मनोहारी 'जय-गणेश' कीर्तन से प्रारम्भ किया करते थे। यदि वहाँ हिन्दी-भाषी श्रोता होते तो वह गुरुदेव के अँगरेजी भाषण का अभिप्राय हिन्दी में समझाने के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित करते थे और श्रोताओं के हृदय का अपहरण कर लेते थे जैसा कि उन्होंने गंगामहल, गया तथा अन्य अनेक स्थानों में किया। जैसा कि इससे पूर्व निर्दिष्ट किया जा चुका है, स्वयं गुरुदेव स्वामी जी की असाधारण विनम्रता, प्राणिमात्र की निस्स्वार्थ सेवा तथा निरन्तर दिव्य चेतना से इतना अधिक प्रभावित थे कि वह जहाँ भी गये, वहाँ सदा ही उन्होंने अपने इस समर्पित शिष्य के आध्यात्मिक गुणों का उल्लेख कर उसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की। चेन्नै के राजभवन में इण्टरनेशनल फेलोशिप (अन्ताराष्ट्रीय मैत्री संघ) को सम्बोधित करते समय उन्होंने एक अनुपम कर्मयोगी के रूप में स्वामी चिदानन्द जी का उदाहरण उद्धृत किया और कहा कि नारायण-भाव से की गयी उनकी सेवा उनसे कहीं अधिक आयु के साधकों के लिए भी एक स्पर्धा-योग्य आदर्श है। उन्होंने चिदानन्द के एक रोगी कुत्ते के उपचार करने की घटना का उल्लेख किया। उसके संक्रमित शरीर से भारी पूतिगन्ध निकलती थी तथा लोगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भगाये जाते रहने के कारण वह सदा चलता रहता था। स्वामी जी ने उसे आश्रम की सीढ़ियों के पास देखा तथा वह कई महीनों तक अपने हाथों से सावधानीपूर्वक उसकी मरहमभट्टी करते रहे। इसी लहजे में गुरुदेव ने भीषण कुष्ठरोग से पीड़ित एक पंजाबी साधु की घटना का उल्लेख किया जिसके पास कोई भी व्यक्ति एक पल भी नहीं ठहर सकता था; किन्तु चिदानन्द जी ने अपने हाथों से उसके कुष्ठपीड़ित हाथों तथा पैरों की मरहमपट्टी कर अपने पवित्र स्पर्श से उसे चमत्कारिक ढंग से स्वस्थ कर दिया। गुरुदेव ने स्वामी जी की अनुकरणीय सेवा के लिए प्रशंसा की भरमार करने के पश्चात् श्रोताओं से प्रश्न किया : "क्या आपमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में एक बार भी ऐसी सेवा की हो?" गुरुदेव के आकलन में स्वामी जी सर्वोत्कृष्ट प्रकार की निस्स्वार्थ सेवा में सर्वातिशायी हैं जिसे वह ऐसी पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा से करते हैं कि वह भगवान् नारायण की पूजा बन जाता है।
गुरुदेव विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में जहाँ-कहीं भी भाषण देते वहाँ स्वामी जी योगासनों के प्रदर्शन करने को अपनी सेवाएँ अर्पित करने के लिए सदा तैयार रहते थे। कभी-कभी वह योगासनों के चलचित्र प्रदर्शन पर चल-विवरण देते थे। अन्नामलै विश्वविद्यालय में गुरुदेव के भाषण के पश्चात् सूर्य-नमस्कार, आसनों, प्राणायामों तथा अन्य यौगिक क्रियाओं के चलचित्र के प्रदर्शन का कार्यक्रम था। स्वामी जी के प्रभावशाली वर्णन से यह चलचित्र प्रदर्शन अपूर्व रीति से सजीव तथा शिक्षाप्रद बन गया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर योगासनों से उद्भूत लाभों को नवयुवकों को समझाया। उस वर्णन ने ऐसा भारी उत्साह उद्दीप्त किया कि प्रकृतार्थ में सैकड़ों छात्र योगासनों को सीखने के लिए आगे आये।
जब यात्रा-मण्डली चिदम्बरम् पहुँची तब गुरुदेव कुछ अस्वस्थ थे। इससे वह सार्वजनिक सभा में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने सभा में भाषण देने के लिए अपने स्थान में स्वामी जी को प्रतिनियुक्त किया। गुरुदेव के एक पुराने सहपाठी कवियोगी शुद्धानन्द भारती भी उनके साथ गये। स्वामी जी सभा-स्थल पर पहुँचे तथा वहाँ उन्होंने अपने आध्यात्मिक उपदेश तथा भावपूर्ण कीर्तन की वृष्टि की। श्रोतागण पुलकित हो गये। गुरुदेव के भाषण के अभाव में उनमें निराशा की भावना नहीं आयी।
यात्रा-मण्डली ८ अक्तूबर को त्रिची पहुँची। स्वामी जी ने स्थानीय राष्ट्रीय महाविद्यालय में अध्यापकों तथा छात्रों के सम्मुख भाषण दिया तथा किस प्रकार हम सब एक ही भगवान् की प्रशाखाएँ हैं, इस मूलभूत सत्य को उन्हें बहुत ही सरल तथा आकर्षक ढंग से समझाया। उन्होंने आत्मसाक्षात्कार के व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया और माना कि एक रत्तीभर अभ्यास मनों सिद्धान्त से श्रेयस्कर है। उन्होंने 'उपदेशामृत' के प्रसिद्ध गान में गुरुदेव के उपदेशों का समाहार किया :
सेवा करो, प्रेम करो, दान करो, शुद्ध बनो,
ध्यान करो और करो आत्मसाक्षात्कार ।
भले बनो, भला करो, सदय बनो और बनो करुणात्मा ।
करो पाला अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का।
यही है योग और वेदान्त का सार ।
प्रश्न करो कौन हूँ मैं, जानो अपनी आत्मा को और बनो मुक्त ।
तुम हो नहीं यह देह और न हो यह मन, तुम हो अमर आत्मा ।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
यात्रा-काल में स्वामी जी को कभी-कभी गुरुदेव की भूमिका अदा करनी पड़ती थी जिसे उन्होंने प्रत्येक अवसर पर आयोजकों तथा भक्तों के परम सन्तोषप्रद रूप से सम्पन्न किया। उदाहरणार्थ, शिवानन्द साधना निलयम, तिरुइंगोमलै के अध्यक्ष स्वामी शंकरानन्द ने गुरुदेव से आश्रम में पधारने तथा आश्रमवासियों को आशीत 'द देने की प्रार्थना की थी; किन्तु गुरुदेव के लिए तिरुइंगोमलै जाना सम्भव न था। तथापि वह आश्रमवासियों को निराश भी करना नहीं चाहते थे। अतएव उन्होंने स्वामी जी को निजी प्रतिनिधि के रूप में उस आदर्श आश्रम को भेजा। वह आश्वस्त थे कि उनका सन्देश उनके योग्य अभिकर्ता के द्वारा शिवानन्द साधना निलयम में कार्यसाधक रूप में पहुँच जायेगा। स्वामी जी ने गुरुदेव के आदेश के अनुसार नियत स्थान को प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचने पर 'साधना निलयम कैसे गुरुदेव की स्वामी अद्वयानन्द को अपरोक्ष प्रेरणा तथा उनके सशक्त सुझाव का परिणाम था, ऐसे आध्यात्मिक केन्द्रा की क्योंकर अपरिहार्य आवश्यकता है और उनका अद्वितीय महत्त्व क्या है तथा गुरुदेव को ऐसी आध्यात्मिक संस्थाओं द्वारा किस प्रकार की अद्भुत आध्यात्मिक क्रान्ति लाना अभीष्ट है' आदि विषयों पर प्रवचन किया। उन्होंने परम विनम्रतापूर्वक श्रोताओं को बतलाया कि वह तो अपने प्रिय गुरुदेव के निमित्त मात्र हैं। इस प्रशस्त भाव से उन्होंने निलयम में रजत कर्णी के साथ प्रस्तावित विद्यालय भवन की आधारशिला रखी, बाद में निलयम के अध्यक्ष स्वामी शंकरानन्द ने अपनी भावना व्यक्त की कि स्वामी जी की पवित्र उपस्थिति तथा उनके प्रेरणादायी भाषण ने वैसा ही वातावरण उत्पन्न किया जैसा कि वे गुरुदेव की उपस्थिति से आशा करते थे।
यात्रा-मण्डली के रामेश्वरम् पहुँचने पर गुरुदेव स्वयं पवित्र गंगाजल को उठा कर ले गये और उसे अभिषेक के रूप में भगवान् शिव को अर्पित किया जब कि स्वामी जी ने भगवान् की स्तुति में स्तोत्रों का पाठ किया तथा रोमहर्षक भजन गाये।
मण्डली ने सागर पार किया तथा वह श्रीलंका द्वीप जा पहुँची। गुरुदेव ने कोलम्बो में एक विशाल सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया। सभा के अनन्तर योगासनों का एक चलचित्र दिखलाया गया। स्वामी जी आसनों के लाभ का चल-विवरण देने के लिए यहाँ पुनः आगे आये। उन्होंने पश्चिमी जगत् के शारीरिक व्यायामों तथा भारतीय योगासनों का साम्य तथा वैषम्य दिखलाया और योगासनों की अधिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया। आसन अन्तःस्रावी तथा अप्रणाल-ग्रन्थियों को कैसे आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित करते हैं, इसका वर्णन किया। उन्होंने और भी संकेत दिया कि अवटु, पीयूष तथा शंकुरूप-ग्रन्थियों की असम्यक् कार्यता को कुछ चुने हुए आसनों के क्रम से सुधारा जाता है।
वापसी यात्रा-काल में त्रिवेन्द्रम में प्रातःकाल एक सत्संग हुआ। स्वयं गुरुदेव की उपस्थिति में स्वामी जी ने ध्यान-क्रम का संचालन किया जिसमें भाग लेने वालों ने उच्चतर ध्यान की मनःस्थिति में अपने को बलात् आकृष्ट तथा तल्लीन होते हुए अनुभव किया। ध्यान-क्रम की समाप्ति पर स्वामी जी ने अन्तरंग साधना के रहस्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने प्रबोधक भाषण में ध्यान में सफलता के लिए साधकों को निम्नांकित सूत्र अपनाने के लिए कहा :
देखो, पर ध्यान न दो।
सुनो, पर कान न दो।
स्पर्श करो, पर स्पर्श-भान न हो।
चखो, पर स्वाद न लो।
स्वामी जी ने आगे कहा कि इस भावना से साधक सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होता और वह शनैः शनैः साक्षी-भाव विकसित करने में सक्षम हो जाता है। एक बार साधक के साक्षी की अभिज्ञा प्राप्त कर लेने पर वह आत्मनिष्ठ हो जाता है और अपने निज-स्वरूप में निवास करता है। इस प्रकार साधक अपने ध्यानाभ्यास में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रबोधक प्रवचन को सुन कर गुरुदेव को अत्यधिक प्रसन्नता हुई तथा उन्होंने स्वामी जी की उनके इस प्रांजल तथा प्रभावकारी प्रतिपादन के लिए सराहना की।
इस भाँति अखिल भारत-यात्रा भर स्वामी जी अपने कोमल स्वास्थ्य की परवाह न कर तथा अपने शरीर पर थोपे गये असाधारण भारी श्रम की पूर्ण उपेक्षा कर गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए प्रत्येक अवसर पर तत्काल बाहर आते तथा उमड़ती हुई भीड़ को सम्बोधित करते, श्रुतिमधुर कीर्तन करते, योगासनों का प्रदर्शन करते तथा उनके लाभ बतलाते और जिज्ञासुओं की शंकाओं को विदूरित करते थे। वह प्रत्येक बार अपने श्रोताओं पर सशक्त प्रभाव छोड़ते थे। उनके प्रवचन, विशेष रूप से ध्यान-विषय के प्रवचन, श्रोताओं को उत्कृष्ट आध्यात्मिक कम्पन से पूरित कर उन पर आश्चर्यकर प्रभाव डालते थे।
इस युगान्तरकारी अखिल भारत-यात्रा की सफलता में स्वामी जी का योगदान निश्चय ही उच्च कोटि का था। उन्होंने एक साधारण से यन्त्र के रूप में गुरुदेव से अपने को सम्बद्ध किया तथा लोगों के मन पर गुरुतर प्रभाव डाला। उनकी विवेचनात्मक-शक्ति, उनका सहजोपलब्ध ज्ञान और सर्वाधिक उनकी अतुलनीय शुचिता तथा विनम्रता ने विपुल संख्या में महाविद्यालय के युवक छात्रों को अपना मिथ्याभिमान परित्याग करने तथा गीता के स्वाध्याय को अपनाने, योगासनों का अभ्यास करने तथा मानव-जाति की सेवा तथा ईश्वर की खोज करने के लिए, आत्मसमर्पण करने को प्रेरित किया।
इस युगान्तरकारी यात्रा में गुरुदेव एक भीमकाय आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में दिखायी पड़े। उन्होंने लोगों को उनकी अकर्मण्यता से प्रबोधित करने के लिए वेदान्त के आदेशों की गरजना की। उनकी उपस्थिति मात्र किसी भी व्यक्ति को पराभूत करने वाली थी। ऐसे आध्यात्मिक महामानव के सम्मुख कोई भी अन्य व्यक्ति नगण्य बन गया होता, किन्तु इस समर्पित शिष्य की अन्तः आध्यात्मिक सम्पत्ति ऐसी थी कि उसने अपनी असाधारण विनम्रता, अनुकरणीय गुरुभक्ति, चुम्बकीय व्यक्तित्व तथा सहजोपलब्ध ज्ञान से सभी के हृदय में अपना विशेष स्थान बना लिया। वह गुरुदेव की उपस्थिति में अपने विषय में जो इतनी प्रशंसा उत्पन्न कर सके वह स्वयं में इनके उस सर्वोच्च आध्यात्मिक आयाम का महत्तम प्रमाण है जिसे वह उस समय तक उपलब्ध कर चुके थे।
चिदानन्द ने भारतवर्ष के लोगों की यह सेवा गुरु-सेवा-कार्य के रूप में की और उन्होंने आज भी वैसा करना बनाये रखा है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार से गुरुदेव के एक यन्त्र के रूप में व्यवहार किया। अनेक स्थानों पर लोगों ने उनके प्रति उतना ही प्रेम तथा समादर प्रदर्शित किया जितना कि स्वयं गुरुदेव के प्रति उनमें था; किन्तु वह अपने ऊपर बरसाये गये सम्मान तथा प्रशंसाओं से रंचमात्र भी कलुषित नहीं हुए। जैसा १९५० में वैसा ही एक पीढ़ी बाद भी उन्होंने गुरुदेव के सेवक के रूप में ही भारतवर्ष के लोगों की सेवा करना जारी रखा है। उन्होंने अपना कोई निजी नया सिद्धान्त रखने का दावा नहीं किया। उन्होंने गुरुदेव की संस्था की सेवा की और उसी में उन्हें परम सन्तोष था। वास्तव में यह अपने लिए तो केवल हिमालय की किसी गुहा में मध्य दीर्घ-कालिक अखण्ड मौन की कामना अपने हृदय में सँजोये हुए थे। यह अभीष्ट आदर्श इस युगान्तरकारी यात्रा-काल में आश्रम के अपने एक घनिष्ठ मित्र के नाम लिखे हुए उनके पत्रों में से एक पत्र में प्रतिबिम्बित होता है। उन्होंने लिखा: "मैं इन मोटरकारों, बड़े बँगलों, दुकानों, नाट्यशालाओं तथा विलासमय वस्त्रधारी लोगों से कुछ ऊब-सा गया हूँ। मैं जीर्ण-शीर्ण तथा मैली-कुचैली धोती पहन कर आश्रम के विश्वनाथ-मन्दिर के पृष्ठभाग के जंगलों में विचरण करने को लालायित हूँ।" ये अल्प-शब्द नाम और यश की दैवायत्त घड़ी में स्वामी जी की अनासक्ति तथा उनके वैराग्य का प्रबल प्रमाण उपस्थित करते हैं। निस्सन्देह यह बहुत बड़े हो-हल्ले में यात्राएँ करते तथा चलते-फिरते थे, किन्तु अपने अन्दर की गहराई में यह प्रशान्त एकान्त के अजेय जगत् में ही निवास करते रहे। व्यस्ततम कार्यक्रम के दिनों में भी यह ध्यान का अपना समय कभी भी हाथ से जाने नहीं देते थे। अनवरत कार्य के बावजूद भी यह अकस्मात् पल मात्र में बाह्य जगत् का परित्याग कर सकते थे। निम्नांकित शब्द, जो स्वामी जी ने यात्रा-काल में अपने एक घनिष्ठ मित्र को लिखे थे, इनकी अन्तर्मुखी अवस्था तथा गम्भीर मौन में आनन्दमय अनुभूति को व्यक्त करते हैं। इन्होंने लिखा : "कल हमने (धनुष्कोटि से श्रीलंका जाते हुए) दो घण्टे जलपोत में व्यतीत किये।... विस्तीर्ण सागर के सम्मोहक जल ने मेरी सम्पूर्ण सत्ता को अपने अधिकार में कर लिया और मुझे बन्दी बनाये रखा। अबाध शान्ति थी। इन्द्रियाँ तथा मन शान्त हो गये थे और मुझे व्यक्तित्व से ऊपर उठा कर किसी ऐसे स्थान में फेंक दिया गया था जहाँ परम नीरवता और उस नीरवता से उत्पन्न मूक आनन्द था। सब-कुछ विस्मृत हो चला था।"
अपनी सत्ता के अन्तर्तम प्रकोष्ठ में इस अभिज्ञा के साथ स्वामी जी गुरुदेव के साथ रहे तथा उन्होंने उनकी तथा भारतवर्ष और श्री लंका के भाग्यशाली नागरिकों की उनके महान् आध्यात्मिक जागरण में सेवा की। वह पद्मपत्र में जल की भाँति व्यवहार करते थे। गुरुदेव शिवानन्द ने भगवान् की आज्ञा का पालन किया और उनके समर्पित शिष्य चिदानन्द ने गुरुदेव के आदेशों को कार्यान्वित किया। दोनों ने ही भारत के साधारण नागरिकों को वेदों के आह्वान को स्मरण कराने तथा उन्हें पुण्य भूमि के ऋषियों तथा मुनियों के भाग्यशाली वंशज होने के नाते धर्मप्रसार के प्रशंस्य कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए स्मरण कराने को उनके द्वार खटखटाये।
पंचम अध्याय
नयी दुनिया (अमरीका) में
"वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।
-सब-कुछ वादेव ही है. (इस प्रकार जो ईश्वर को भजता है) वह महात्मा अति-दुर्लभ है"
(गीता : ७-१९)।
सन् १९५० की युगान्तरकारी अखिल भारत-यात्रा से स्वामी जी सनातन धर्म के एक विशिष्ट सन्देशवाहक के रूप में उभर कर सामने आये। गुरुदेव को, जो आधुनिक जगत् के लिए चिदानन्द के महत्त्व के विषय में कई बार भविष्यवाणी कर चुके थे, अपने उस विश्वास को सत्य सिद्ध होते हुए पा कर प्रसन्नता हुई। वह पहचान सके थे कि पाश्चात्य जगत् में भारतवर्ष का सनातन सन्देश ले जाने के लिए स्वामी जी ही सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं। उनके दिव्य जीवन का सुसमाचार विश्व में चतुर्दिक् पहुँचाने तथा उसके मुख्य व्याख्याता तथा आदर्श होने के लिए उनके शिष्यों में वह ही सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप से उपयुक्त हैं।
परन्तु स्वामी जी का अपने लिए बहुत ही भिन्न कार्यक्रम था। हिमालय की विरल ऊँचाइयों में अतिचेतना की आनन्दमय अवस्था में सदा रहने के प्रयास में वह एकान्त जीवन की ओर शनैः-शनैः अधिकाधिक खिंचते जा रहे थे। इस भाँति वे गुरुदेव की अनुमति से सन् १९५८ की ग्रीष्म ऋतु में बदरीनारायण चले गये और वहाँ आभ्यन्तरिक मौन में कई महीने रुके। मन्दिर को शीत ऋतु के लिए बन्द होना था, अतः स्वामी जी दिसम्बर में नीचे आश्रम वापस आ गये; किन्तु यह तब भी इतने अन्तर्मुखी तथा एकान्तसेवी बने रहे कि गुरुदेव ने इन्हें उत्तरकाशी जाने का परामर्श दिया तथा काली कमली वाला क्षेत्र के प्रबन्धक से स्वामी जी को उपयुक्त आवास प्रदान कराने के लिए उत्तरकाशी में अपनी संस्था के शाखा प्रबन्धक को पत्र लिखने के लिए अनुरोध किया। गुरुदेव ने यह व्यवस्था ३१ दिसम्बर १९५८ को की; किन्तु यह मूर्तरूप लेने वाली न थी। इस योजना में आकस्मिक परिवर्तन हुआ। स्वामी राधा, जिन्होंने बैंकूवर में शिवानन्द-आश्रम स्थापित कर रखा था, इसी बीच आनन्द-कुटीर पधारी तथा उन्होंने बैंकूवर-आश्रम के जिज्ञासुओं को प्रेरणा देने तथा उनका पथ-प्रदर्शन करने के लिए अपने वरिष्ठ संन्यासी शिष्यों में से किसी एक को वहाँ जाने तथा तीन-चार माह तक रुकने के लिए कहने को गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव ने उन्हें आवश्यक व्यवस्था करने का विश्वास दिलाया। अतः उन्होंने स्वामी जी के विषय में अपनी योजना में सुधार कर उन्हें वैंकूवर भेजने का विचार किया; क्योंकि वह दिव्य जीवन के सर्वाधिक सुसंस्कृत तथा योग्य सन्देशवाहक थे। वह जानते थे कि स्वामी जी के लिए, जो उत्कृष्ट कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान तथा सन्तुलन प्राप्त कर चुके हैं, कनाडा अथवा उत्तरकाशी से कोई अन्तर नहीं पड़ता। अतः उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया और पश्चिमी गोलार्ध में योग तथा वेदान्त के सन्देश का प्रचार करने के लिए कनाडा जाने के लिए कहा। ग्वामी जी ने गुरुदेव को विनम्रतापूर्वक स्मरण दिलाया कि उत्तरकाशी जाने के लिए उनके लिए पहले से ही प्रबन्ध किया जा चुका है; किन्तु गुरुदेव ने केवल इतना ही कहा- "भगवत्-कार्य भला है।" इस प्रकार उन्होंने स्वामी जी को स्मरण दिलाया कि उनका जन्म एक महत् उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्व तथा पश्चिम के मानवों का उत्थान करने के लिए हुआ है। स्वामी जी गुरुदेव के सम्मुख नतमस्तक हुए और मन-ही-मन गुनगुनाया -"प्रभु! तेरी इच्छा पूर्ण हो ।'' इस भाँति निस्स्पृह महात्मा जिसने एकान्त में अखण्ड ध्यान के लिए अपने को अर्पित कर देने का निश्चय कर लिया था, अब भगवान् तथा गुरुदेव की इच्छा के परिपालन में अमरीका की व्यापक यात्रा आरम्भ करने को प्रेमपूर्वक सहमत हो गया।
किन्तु स्वामी राधा गम्भीर रूप से रुग्ण हो गयीं तथा उनकी यात्रा का आवश्यक प्रबन्ध न कर सकीं और उन्हें गुरुदेव की इच्छानुसार आश्रम में समय की प्रतीक्षा करते रहना पड़ा। गुरुदेव की एक अन्य भक्त महिला अमरीका के मिल्वाकी नगर की श्रीमती विक्टोरिया कोयण्डा ने, जो पहले आश्रम आ चुकी थीं, इसी बीच यह सुना कि स्वामी जी के कनाडा आने की कुछ सम्भावना है। उन्होंने स्वेच्छा से मार्ग-व्यय भेज दिया तथा गुरुदेव से स्वामी जी को किसी प्रकार से भेजने की प्रार्थना की। अतः गुरुदेव ने स्वामी जी को श्रीमती कोयण्डा का निमन्त्रण स्वीकार करने तथा प्रथम अमरीका और तत्पश्चात् कनाडा जाने का परामर्श दिया। यह दैवकृत व्यवस्था थी जो स्वामी जी को उत्तरकाशी के स्थान पर अमरीका ले गयी। स्वामी जी ने यथासम्भव न्यूनातिन्यून निजी सामान तथा गुरुदेव के उत्कृष्टतम आशीर्वाद के साथ ३० अक्तूबर को आश्रम से प्रस्थान किया। संयुक्त राज्य अमरीका के लिए विदा होने की पूर्व-सन्ध्या ३१ अक्तूबर को नयी दिल्ली के कान्स्टीट्यूशन क्लब हाल में स्वामी जी ने एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया। पाश्चात्य देशों के नाम शिवानन्द के सन्देश की चर्चा करते हुए उन्होंने पुलकित स्वर से भाषण समाप्त किया-"हे मानव! आप तत्त्वतः दिव्य हैं। ईश्वर-परायणता आपमें अन्तर्विष्ट है। आप इस संसार के नहीं हैं, मृण्मय नहीं हैं। आप सच्चिदानन्द के प्रकाश की दीप्ति से पूर्ण आत्मा हैं। वही आपका परम स्रोत है, आपका अन्तरतम सत्त्व है और आपका प्रशस्य चरम लक्ष्य है।"
स्वामी जी ने २ नवम्बर १९५९ को दिल्ली से वायुयान द्वारा अमरीका को प्रस्थान किया। मार्ग में वह केयरो में रुके जहाँ दिव्य जीवन संघ की स्थानीय शाखा के मुहम्मद अब्दुल्ला अल मेंहदी ने उनका स्वागत किया। इसी भाँति इस्तानबुल में पत्रकार अलरिज़ा आकिशां ने इनका स्वागत किया। इस्तानबुल के अधिकांश समाचारपत्रों ने इनके आगमन का व्यापक प्रचार किया। स्वामी जी से पत्रकारों तथा तुर्की के एक प्रमुख समाचार फिल्म संस्थान एडीसी ने भेंटवार्ता की। यहाँ इन्होंने इस्तानबुल उच्च विद्यालय में योगासनों का प्रदर्शन किया तथा इस यात्रा का अपना प्रथम सार्वजनिक भाषण दिया। यहाँ इन्होंने छात्रों को आदर्श जीवन-यापन करने तथा निर्दोष चरित्र निर्माण करने की प्रेरणा दी। स्वामी जी ने न्यूयार्क जाते हुए मार्ग में रोम, डसेल्डोर्फ तथा लन्दन में विराम किया। जब यह न्यूयार्क पहुँचे तो इन्होंने स्वामी विष्णुदेवानन्द को हवाई पत्तन पर प्रतीक्षा करते हुए देखा। गुरुदेव शिवानन्द के शिष्य तथा इनके गुरुभाई स्वामी विष्णु ने हठयोग के प्रचार के लिए अमरीका के विभिन्न भागों में शिवानन्द योग-वेदान्त-केन्द्र खोल रखे हैं। स्वामी चिदानन्द जी महाराज ने कार्निश आर्म्स होटल के योग-वेदान्त-केन्द्र में रुक कर तीन प्रवचनों की शृंखला में १८, २० तथा २१ तारीख को क्रमशः 'राजयोग', 'हिन्दू-दर्शन में माया की संकल्पना' तथा 'कर्म और पुनर्जन्म' विषयों पर प्रवचन किये। यह श्रोताओं के लिए एक असाधारण अनुभव था। जब वे सशक्त वाग्मिता तथा तर्क के शिखर पर पहुँच रहे थे उसी समय उन्होंने श्रद्धेय स्वामी जी द्वारा प्रजनित अतिबृहत् आध्यात्मिक शक्ति अनुभव की जिसने एक तर्कातीत ढंग से उनकी सम्पूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया। यह श्रोताओं में से प्रत्येक के लिए 'मैं आया, मैंने देखा, मैं विजित हुआ' का रोमांचकारी उदाहरण था।
स्वामी जी ने २६ नवम्बर को न्यूयार्क से वायुयान द्वारा प्रस्थान किया और उसी दिन मिल्वाकी (विसकान्सिन) पहुँच गये जहाँ श्रीमती तथा श्रीमान् कोयण्डा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। इस महान् भारतीय योगी के आगमन पर मिल्वाकी के दैनिक ने समाचार प्रकाशित किया कि शिवानन्द का आध्यात्मिक सन्देशवाहक योग तथा वेदान्त के प्रचार के लिए अमरीका पहुँच गया है।
स्वामी जी २ दिसम्बर १९५९ को अमरीका में प्रथम बार दूरदर्शन-तन्त्र पर आये और उसके शीघ्र बाद ही उन्होंने आकाशवाणी पर 'दिव्य जीवन के सुसमाचार' विषय पर भाषण दिया। उन्होंने बताया कि सत्य, अहिंसा तथा शुचिता धर्म तथा आध्यात्मिकता के सार हैं। वे योग तथा वेदान्त के भी सार हैं। निस्स्वार्थ सेवा, वैश्व प्रेम, उदारता, शुचिता, उपासना तथा ध्यान अपने-आपसे तथा अचूक रूप से प्रबोध तथा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करायेंगे। इस प्रकार उन्होंने अमरीकावासियों को गुरुदेव शिवानन्द के सुसमाचार के विषय में बतलाया और अपने व्यक्तिगत सम्पर्क में अपनी गम्भीर निष्कपटता, परम शुचिता तथा गहरी विनम्रता से उन्हें प्रभावित किया।
स्वामी जी ने ६ दिसम्बर को मिल्वाकी के योग-वेदान्त-केन्द्र की प्रथम सभा में भाषण दिया और योग के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए लगभग सौ जिज्ञासुओं को समाकृष्ट किया। उन्होंने १४ दिसम्बर को एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम आरम्भ किया। यह सूर्यनमस्कार, योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान का दैनिक वर्ग चलाते थे। इन्होंने इन वर्गों की पाठ्यपुस्तक के रूप में गुरुदेव की अँगरेजी पुस्तक 'राजयोग के चौदह पाठ' को अपनाया और यह अपने निजी विलक्षण रूप से उन्नतकारी तथा अप्रतिम शैली में पुस्तक के भावों को समझाते थे। यह ६०७, कालेज ऐविन्यू में श्रीमती तथा श्रीमान् कोयण्डा के निवास स्थान पर भी ध्यान का दैनिक वर्ग चलाते थे। स्वामी जी की पवित्र उपस्थिति से आतिथेय अवर्णनीय आनन्द से परिपूर्ण थे। मिल्वाकी में उनके प्रवचनों के विषय थे-'ईसाइयों के लिए योग', 'योग तथा आत्मोत्थान', 'नव-जीवन' तथा 'ध्यानाभ्यास' । किवानिस क्लब तथा साउथ मिल्वाकी पब्लिक स्कूल में इन्होंने 'योग में मनोविज्ञान', 'जीवन के प्रति हिन्दुओं का दृष्टिकोण', 'वैदिक संकल्पनाएँ तथा आदर्श' तथा 'नवयुवकों के लिए महत्त्वपूर्ण आदर्श' विषयों पर भाषण दिये। इन सभी भाषणों में न तो बौद्धिक इन्द्रजाल था और न ही रहस्यवाद की दुर्बोधता। वे इनके निजी वैयक्तिक अनुभवों पर आधारित तथा उनके द्वारा प्रमाणित थे तथा उनमें बहुत ही व्यावहारिक तथा सीधे-सादे निरूपण तथा अनुदेश समाविष्ट थे। मिल्वाकी के अपने आवास-काल में यह श्रीमती विक्टोरिया की बहन श्रीमती वीरा बर्च के घर गये थे। वहाँ उन्होंने ३६२०-ई, अण्डरवुड ऐविन्यू, कुडाही, विसकान्सिन में दो विशेष सत्संगों में अपना धर्मोपदेश दिया। पत्रकार तथा लेखिका डोरोथी मैडल बाद के अपने अतीत के मधुर दिनों के संस्मरणों में लिखती हैं : "अपने पारम्परिक परिधान में यह कृशकाय संन्यासी कोयण्डा की बैठक में सन्तोषपूर्वक बैठे हुए निरभिमान रूप से प्रश्नों के उत्तर देते थे। स्वामी जी ने बताया कि अब योग में गोपनीयता की आवश्यकता नहीं रही। योग धर्म नहीं है। यह भगवान् के निकटतर जाने की एक प्रविधि है।" जनवरी ११६० के मध्य में स्वामी जी मिन्निमापोलिस गये जहाँ इन्होंने 'भारत की आध्यात्मिक संस्कृति तथा आधुनिक मानव के जीवन में उसकी प्रासंगिकता' पर पाँच भाषण दिये । भाषणों के इस कार्यक्रम की व्यवस्था नवयुवक क्रिश्चियन संघ ने की थी तथा इनमें लोगों की उपस्थिति अच्छी रही।
प्राच्य-पाश्चात्य सांस्कृतिक केन्द्र के डा. जूडिथ टाइबर्ग के अनुरोध पर स्वामी जी ७ फरवरी १९६० को लास ऐंजिलेस गये और वहाँ एक मास तक रुके। इस अवधि में उन्होंने अमरीकावासियों पर अत्यधिक आध्यात्मिक प्रभाव डाला। प्राच्य-पाश्चात्य सांस्कृतिक केन्द्र, ११६२, नार्थ स्ट्रीट, एण्डूस पी. एल. में 'योग-विषयक क्या और क्यों का प्रश्न' पर उनके भाषण ने अत्यधिक हलचल तथा आध्यात्मिक उद्बोधन उत्पन्न किया तथा अनेक प्रतिष्ठित तथा विद्वान् लोगों ने यह स्वीकार किया कि स्वामी जी एक असाधारण आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। इसी अवधि में एक सच्चे जिज्ञासु पीटर मन ने जो स्वामी जी से मिले, लिखा- 'भारत से यहाँ आये हुए स्वामी चिदानन्द पर दृष्टिपात करते ही आप यह समझ जायेंगे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, किन्तु यह विचार उनके काषाय रंग के संन्यासी परिधान अथवा उनके बारीक कटे केश के कारण नहीं उत्पन्न होता है और न उनके दुष्कर पद्मासन में बैठने के कारण उत्पन्न होता है वरन् यह निश्चय ही उनके नेत्रों के-विशाल, श्यामल तथा चमकीले नेत्रों के कारण उत्पन्न होता है। उनमें गम्भीर रहस्यमयी गम्भीरता प्रतिबिम्बित होती है।" लास ऍजिलेस के अपने प्रवचनों में स्वामी जी ने अपना मत व्यक्त किया कि योग धर्म से परे है और जो भी ईश्वर में विश्वास करता है उसे वह प्राप्य है। उन दिनों स्वामी जी का नाम प्रत्येक व्यक्ति के ओष्ठों पर था। २२ फरवरी को 'लास ऐंजिलेस इग्जैमिनर' समाचार-पत्र ने अपने सोमवार के अंक में स्वामी जी की वाग्मिता की प्रशंसा करते हुए संवाद प्रकाशित किया। उसने स्वामी जी की व्याख्या के अद्भुत प्रभाव पर टिप्पणी की : "जिस समय आप प्राच्य-पाश्चात्य सांस्कृतिक केन्द्र में स्वामी चिदानन्द से वार्ता करते हैं, वह योग-विषयक क्या और क्यों के प्रश्न का रहस्य उद्घाटित करते हैं।”
श्रीमती मेटा थर ओल्सन,जो स्वामी शिवानन्द को पहले से ही जानती थी चिदानन्द से इतना अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने गुरुदेव को लिखा: "मैं आपको यह भी बतला देना चाहती हूँ कि केनिथ तथा मैं स्वामी चिदानन्द से अत्यधिक सानुकूल रूप से प्रभावित हुई है। हम अनुभव करती है कि यदि आप स्वयं इस समय अमरीका नहीं आ सके तो आपने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए यथासंभव उत्कृष्टतम संदेशवाहक भेजा। जब कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति के बाह्य परिधान के नीचे डॉंकताहै तो वह यहाँ अनेक सदगुणों से सम्पन्न एक बहुत ही साधु आत्मा के दर्शन करता है। इनमें प्रभु के प्रति कितनी अगाध भक्ति है और कितने निष्कपट हैं यह। मैंने इन्हें अपने घर में ध्यान से देखा तथा इनके भाषण को सुनने पर यह अनुभव किया कि यह अपने प्रिय गुरुदेव के प्रतिबिम्ब हैं।...उनसे परिचित होना निश्चय ही बड़े सद्भाग्य की बात है। मैं ठीक-ठीक इनकी प्रशंसा नहीं कर सकती ।... इन्हें यह पता नहीं है कि यह सब सुन्दर बातें आपको बतलाने के लिए पत्र लिख रही हूँ। यह इतने विनम्र तथा भाग्यशाली आत्मा है कि मुझे विश्वास है कि यह आपको स्वयं कभी नहीं यथासम्भत बतला सकेंगे।"
स्वामी जी लास ऍजिलेस के अपने आवास-काल में माउण्ट वाशिंगटन में सेल्फ रिअलाइजेशन फेलोशिप (Self Realisation Fellowship) का प्रमुखालय भी देखने गये जहाँ यह सेल्फ रिअ रिअलाइजेशन फेलोशिप की अध्यक्षा संघिनी दया माता के अतिथि थे। संघिनी दया परमहंस योगानन्द की, जो अमरीका में क्रियायोग को लोकप्रिय बनाने में बहुत सफल रहे थे, शिष्या हैं। वह स्वामी जी के दिव्य व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुई कि गुरुदेव शिवानन्द को लिखने को प्रेरित हुईं : "आपके निष्ठावान् चेले श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज हमारे यहाँ भी आये हैं और इस समय एन्सीनिटास में हमारे आश्रम में कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए हैं। हम उन्हें अपने मध्य पा कर अत्यधिक प्रसन्न हैं; क्योंकि उनकी विनम्रता, सरलता तथा शुचिता ने हमारे हृदय को जीत लिया है। वह हम लोगों तक ऋषिकेश के गंगा-तट से दिव्य जीवन का नवीन प्रेरणाप्रद संस्पर्श भी लाये हैं।"
स्वामी जी लास ऍजिलेस में लगभग एक माह तक योग के वर्गों का संचालन करते तथा योग तथा वेदान्त पर भाषण देते रहे थे। तत्पश्चात् वह सैन फ्रान्सिस्को गये जहाँ उन्होंने एक माह दिव्य जीवन के सन्देश के प्रचार में लगाया। इन औपचारिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, स्वामी जी से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने समालाप किया जिसका उन पर अमिट प्रभाव पड़ा। सैन फ्रान्सिस्को के उनके आवास-काल की ऐसी ही एक वैयक्तिक भेंट स्मरण है जब वह एक जर्मन महिला माता पौला कोर्नेली को, जो एक उत्कृष्ट भक्त तथा निष्कपट साधक थीं, दर्शन देने लिए जेम्स टाउन गये। यह बहुत ही रोचक मिलन था। इधर पौला माता उनके सौजन्य से सम्भ्रान्त तथा अत्यधिक प्रभावित अनुभव कर रही थीं और उधर स्वामी जी उनसे पूर्व-परिचित की भाँति परम विनीत भाव तथा प्रसन्न चित्त से मिल रहे थे तथा उनके साथ बहुत ही स्वाभाविक तथा सहज व्यवहार कर रहे थे। इस अल्पकालिक भेंट का प्रभाव यह कालान्तर में स्मरणीय बनना था। पौला माता ने अपने को सेवा तथा साधना के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि जब क्षेत्र तैयार होता है हो तो बीज भी तैयार होता है और गुरु उपयुक्त समय पर व्यक्ति की देहली पर आ जाता है।
स्वामी जी ने १३ अप्रैल को सैन फ्रान्सिस्को से प्रस्थान किया और अल्पकाल तक पोर्टलैण्ड में ठहरने के पश्चात् वह माण्ट्रियल पहुँचे। माण्ट्रियल में उन्होंने शिवानन्द योग-वेदान्त-केन्द्र, २०२९ स्टैनली स्ट्रीट के निर्देशक स्वामी विष्णुदेवानन्द की अनुपस्थिति में केन्द्र की प्रवृत्तियों का संचालन किया। यहाँ उन्होंने योग तथा भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों पर शृंखलाबद्ध भाषण दिया। माण्ट्रियल से १९ मई को उन्होंने वैन्कूवर बी. सी. को प्रस्थान किया जहाँ स्वामी राधा (श्रीमती हेल्मन) तथा अन्य भक्तों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। यहाँ शिवानन्दाश्रम, साउथ बर्नबाई के उपनगर के ६५९१ मार्लबरो ऐविन्यू में उन्होंने ध्यान के नियमित वर्ग चलाये तथा योग के विभिन्न अंगों पर शृंखलाबद्ध प्रवचन किया। उन्होंने पतंजलि के योगसूत्र, भगवद्गीता तथा उपनिषद् की अपने अनुभव की दृष्टि से शिक्षा दी। उन्होंने कनाडा के इस पश्चिमी भाग में मध्य अगस्त तक गुरुदेव की संस्था की सेवा की और तत्पश्चात् वह अपने गुरुदेव के अनुदेश से अगस्त के तृतीय तथा चतुर्थ सप्ताह में अपने निजी उद्देश्य से पश्चिमी जर्मनी गये।
अगस्त माह के अन्त में वह जर्मनी से प्रस्थान कर लास ऐंजिलेस पहुँच गये। उन्होंने हालीवुड में प्राच्य-पाश्चात्य सांस्कृतिक केन्द्र के तत्त्वावधान में 'योग के मूलतत्त्व' तथा 'जीवन की आध्यात्मिक मान्यताएँ' विषय पर शृंखलाबद्ध दश भाषण दिये । तत्पश्चात् अल्पकालिक विश्राम के लिए वह वैंकूवर चले गये। स्वामी जी की ख्याति अब तक इस विस्तीर्ण देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गयी थी। एशियन अध्ययन के अमरीकी विद्यापीठ ने उन्हें एक अतिथि प्राध्यापक के रूप में शृंखलाबद्ध भाषण देने के लिए सैन फ्रान्सिस्को आने के लिए आमन्त्रित किया। अतएव वह बैंकूवर से सैन फ्रान्सिस्को चले गये और वहाँ उन्होंने एशियन अध्ययन के अमरीकी विद्यापीठ के छात्रों को वेदान्त तथा भारतीय कुल-परम्परा पर व्याख्यान देते हुए चार मास व्यतीत किये। सैन फ्रान्सिस्को में अपने इस चार माह के आवास की अवधि में उन्होंने वर्गों के संचालन तथा भाषण के बहुत ही उपयोगी तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम रखे। वह सप्ताहान्त बिताने के लिए परम भक्त पौला माता के अतिथि के रूप में कभी-कभी जेम्स टाउन जाया करते थे। जेम्स टाउन में ऐसे अभ्यागमनों के समय पौला माता का आवास एक आश्रम का रूप ले लेता तथा आध्यात्मिक स्पन्दनों से भर जाता था। स्वामी जी यहाँ अपना सम्पूर्ण समय प्रवचनों, सत्संगों, सामूहिक ध्यान, योगासनों के वर्ग तथा बहुसंख्यक जिज्ञासुओं के सन्देह-निवारण के साक्षात्कारों में लगाया करते थे। उन्होंने दो बार स्थानीय नगर-भवन में भाषण दिया। अधिक प्रचार के बिना भी भवन विपुल श्रोताओं से आश्चर्यकर रूप से भर जाता था। वहाँ पर एकत्र होने वाले जिज्ञासुओं के लिए एक भगव, साक्षात्कार-प्राप्त आत्मा के सम्पर्क के माध्यम से आध्यात्मिक स्पन्दन का यह अनूठा अनुभव था। स्वामी जी अपनी शालीनता तथा ज्ञान के कारण उन सबके प्रेम-पात्र बन गये।
स्वामी जी ने इन सत्संगों का आयोजन करने वाली ब्रह्माण्डीय योजना का उल्लेख करते हुए पौला माता को लिखा: “यदि उस (विधि) की इच्छा तथा आपके प्रायः अनवरत स्मरण के पुण्य का बल न होता तो पश्चिमी जगत् में आने पर मैं प्रत्येक बार ही जेम्स टाउन बारम्बार आने को क्योंकर विवश होता?" स्वामी जी के प्रति माता पौला की भक्ति की गाथा निस्सन्देह अद्वितीय तथा रोमांचकारी है। उन पर स्वामी जी का ऐसा भारी प्रभाव पड़ा कि बाद में स्वामी जी के अमरीका से प्रस्थान करने पर उन्होंने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति बेच डाली तथा समस्त सांसारिक सुखों को तिलांजलि दे कर शिवानन्दाश्रम आ गर्थी। वहाँ उन्होंने परमाध्यक्ष के कुटीर के पास 'ॐ कुटीर' का निर्माण करवा कर अपना सारा समय पशुओं की सेवा तथा ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत किया। अपने अन्तिम दिनों में उनकी एकमात्र इच्छा यह थी कि मृत्यूपरान्त उनके शब को स्वयं स्वामी जी गंगा में विसर्जित करें। स्वामी जी ने रोमांचकारी परिस्थितियों में उनकी इस अन्तिम इच्छा को पूर्ण किया। इस भाँति चाहे पूर्व में हों या पश्चिम में, वह केवल औपचारिक कार्यक्रमों में ही नही बल्कि विशिष्ट भक्तों तथा जिज्ञासुओं में गहरी दिलचस्पी लेते थे। स्वामी जी ने सैन फ्रान्सिस्को से लास ऐंजिलेस को प्रस्थान किया। तत्पश्चात् वह सन् १९६१ के प्रारम्भ में हास्टेन (टेक्साज़), मिल्वाकी (विस्कान्सिन) तथा कुछ अन्य नगरों में गये तथा इन सभी स्थानों में उन्होंने गुरुदेव के सन्देश का प्रचार किया। तब वह शिवानन्द योग-वेदान्त-केन्द्र में अल्पकालिक निवास के लिए माण्ट्रियल गये। स्वामी जी ने उत्तरी अमरीका में लगभग डेढ़ वर्ष तक योग-वेदान्त की शिक्षा दी। तत्पश्चात् मार्च १९६१ में वे माण्ट्रियल से प्रस्थान कर न्यूयार्क और लन्दन में से प्रत्येक में एक सप्ताह रुके। लन्दन से उन्होंने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में स्विट्ज़रलैण्ड को प्रस्थान किया। यहाँ पर उन्होंने एक माह तक प्रवचन किया तथा सेण्ट गाल के निकट ट्रोजन में ईस्टर आध्यात्मिक साधना-शिविर का संचालन किया।
तत्पश्चात् उन्होंने ज़्यूरिक, बैसेल तथा बर्न में सार्वजनिक भाषण दिये। स्वामी जी कैथोलिक पुजारी सन्त पैड्रेपियों के दर्शन करने के लिए स्विट्जरलैण्ड से इटली गये। यह ईसाई आचार्य फ्रान्सिस्कन सन्त थे। इनके पाँच-दोनों हाथों, दोनों पैरों तथा शरीर के एक ओर क्षत-चिह्न थे। उन्होंने ईसा की पीड़ाओं से अपना तादाम्त्य किया था; उसी से इनके शरीर में पाँच क्षत-चिह्न हो गये। जब स्वामी जी ने आचार्य का दर्शन किया तब वह पर्याप्त वृद्ध हो चुके थे, सत्तर-अस्सी वर्ष की आयु के थे। इन वरिष्ठ सन्त ने नवयुवक भारतीय स्वामी के प्रति शिष्टता दिखलायी। स्वामी जी ने उनसे उनके आशीर्वाद की याचना की तथा उनकी इस अल्पकालिक संगति से अत्यधिक सन्तोष अनुभव किया। भागवत पुरुष अपने मन तथा शरीर को भगवान् में पूर्णतया विलीन रखते हुए इसी प्रकार एक-दूसरे की कदर करते तथा एक-दूसरे को उद्बुद्ध करते हैं। इटली से स्वामी जी लन्दन गये। तत्पश्चात् वह पुनः न्यूयार्क गये जहाँ कुछ दिनों तक विराम करने के पश्चात् उन्होंने दक्षिणी अमरीका के लिए प्रस्थान किया।
वह २१ मई १९६१ को माण्टेवीडियो पहुँचे तथा २७ जुलाई को उन्होंने दिव्य जीवन संघ की माण्टेवीडियो शाखा का उद्घाटन किया। यहाँ चार महीने रुक कर उन्होंने सामूहिक ध्यान-सहित योग के विभिन्न पहलुओं पर नियमित वर्ग का संचालन किया। गुरुदेव के परम भक्त डा. ओलैण्डो पी. डाल स्वामी जी की दक्षिणी अमरीका की यात्रा के प्रमुख आयोजक थे। माण्टेवीडियो में स्वामी जी के आवास-काल में उरुगुई के तत्कालीन उप-विदेशमन्त्री डा. मैटियो जे. एम. मैगरिनोस स्वामी जी की आध्यात्मिक प्रभा से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी शिक्षाओं में गहन रुचि ली। स्वामी जी की उरुगुई की यात्रा ३० सितम्बर १९६१ को समाप्त हुई। माण्टेवीडियो शिवानन्द-केन्द्र के जिज्ञासुओं तथा छात्रों ने उन्हें हृदयस्पर्शी विदायी दी। अलेक्जेण्डर एरु तथा उनके मित्रों के आमन्त्रण पर स्वामी जी ब्यूनिस आयर्स में योग के वर्ग तथा आध्यात्मिक प्रवचन के पंच-दिवसीय कार्यक्रम के लिए अर्जेन्टाइना गये।
वह ५ अक्तूबर १९६१ को वायुयान द्वारा अमरीका वापस लौटे तथा ६ तारीख को हास्टन (टेक्साज़) में उतरे। यहाँ उन्होंने तीन दिन तक सत्संग चलाया। श्री वैरी टिंकलर तथा प्रोफेसर अर्नेस्ट वुड ने भाषण के कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा स्वामी जी के आतिथेय रहे। तत्पश्चात् स्वामी जी सैन ऐन्टोनियो गये जहाँ उन्होंने प्रख्यात प्राकृतिक स्वास्थ्य-विज्ञानी डा. हर्बर्ट शेल्टेन से भेंट की। तत्पश्चात् वह प्राच्य-पाश्चात्य सांस्कृतिक केन्द्र के डा. जूडी टाइबर्ग के अतिथि के रूप में कैलीफोर्निया गये। मैरियो, ब्रोडाइन, टाम डैनेली, इना सेलिन, प्रूस, श्रद्धेय रेमर, श्रद्धेय गौन्ट, गुनर वाल्टर आदि अनेक सच्चे जिज्ञासु तथा पुराने भक्त स्वामी जी से मिलने तथा उनकी ज्ञानमयी वाणी सुनने के लिए लास ऐंजिलेस में एकत्रित हुए। स्वामी जी ने एक प्रार्थना-सभा में अपने उन्नतकारी भाषण से साधकों को प्रेरित किया तथा ध्यान का एक वर्ग चलाया।
लास ऐंजिलेस से वह २० अक्तूबर १९६१ को सैन फ्रांसिस्को पहुँचे और अगले दिन माता पौला कार्नेली तथा उनकी आध्यात्मिक गोष्ठी को दर्शन देने तथा वहाँ के जिज्ञासुओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए जेम्स टाउन गये। माता पौलां की अनवरत प्रार्थना ही उन्हें उस स्थान पर खींच लायी। जैसा कि स्वामी जी ने जिस रहस्यमय ढंग से उनकी अकथित किन्तु भक्तिमयी प्रार्थना को प्रायः स्वीकार करते थे उसके विषय में बतलाते हुए उन्होंने बाद में उन्हें लिखा : "मैं आपके पास ही हूँ। मैं अनादि-अनन्त-अन्तर्यामी के अंग के रूप में, जिससे मैं आत्मरूप में अभिन्न हूँ, आपके अन्दर निवास करता हूँ।" मुक्त वातावरण में धूप वाले शरत्कालीन आकाश के नीचे उन्होंने भक्तों को चिन्तनशील मनोदशा से आपूरित कर दिया तथा उन्हें अपनी प्रार्थना के द्वारा आशीर्वाद दिया। सैन फ्रांसिस्को वापस आ कर स्वामी जी ने वहाँ के मेटाफिज़िकल टाउन हाल में दिव्य जीवन संघ के भक्तों को पुनः सम्बोधित किया तथा कुछ वैयक्तिक साक्षात्कारों में छात्रों तथा जिज्ञासुओं की शंकाओं को स्पष्ट किया।
सैन फ्रांसिस्को से उन्होंने पोर्टलैण्ड (ओरेगन) के लिए प्रस्थान किया जहाँ वह वेदान्त सोसायटी के श्री स्वामी अशेषानन्द जी से मिले और तत्पश्चात् बैंकूवर चले गये। बैंकूवर में स्वामी राधा, बिल ईलर्स, जो, हेल, कैरोल, श्रद्धेय प्रीस्टली, फ्रेड ब्लैक आदि भक्त एक रविवार को एकत्रित हुए और ६ नवम्बर १९६१ को स्वामी जी के आशीर्वादात्मक प्रवचन में अन्तर्विष्ट ज्ञान-निर्झर में गहराई से पान किया। स्वामी जी बैंकूवर से इवोवा गये जहाँ वह डा. आर. होलजिगर के अतिथि के रूप में रुके और एक प्रार्थना-सभा में भक्तों को अनुप्राणित किया। इवोवा से उन्होंने मिन्नेपोलिस को प्रस्थान किया। वहाँ दो सत्संगों में सम्मिलित हुए। तत्पश्चात् वह १० नवम्बर को मिल्वाकी गये जहाँ वह श्री जोसेफ तथा श्रीमती विक्टोरिया कोयण्डा के अतिथि के रूप में चौदह दिन ठहरे। यहाँ वह ऋषिकेश आश्रम के स्वामी शिवप्रेमानन्द से मिले जो उस समय मिल्वाकी आये हुए थे। उन्होंने २३ नवम्बर १९६१ को मिल्वाकी के भक्तों से विदा ली और न्यूयार्क के लिए प्रस्थान किया जहाँ वह चार दिन रुके तथा योग-वेदान्त-केन्द्र के छात्रों को सम्बोधित किया। वह अमरीका से २७ नवम्बर को विदा हो कर मांट्रियल पहुँचे जहाँ वह स्वामी विष्णुदेवानन्द से मिले। यहाँ उन्होंने ३० नवम्बर तथा १ दिसम्बर को दो सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिये।
स्वामी जी ने १ दिसम्बर १९६१ को नयी दुनिया (अमरीका) से प्रस्थान किया और अब वह गृहाभिमुख हुए। प्रत्यागमन के समय वह पैरिस में रुके तथा वहाँ से लगभग ५०० मील दूर स्थित लाउडेंस के पवित्र देवायतन की यात्रा की। लाउडेंस में एक चमत्कारक जलस्रोत है जिसमें रोगमुक्ति के लिए गोता लगाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में विकलांग व्यक्ति जाते हैं। यह देवायतन मरियम माता के अभ्यागमन से पुण्य तीर्थ बन गया है। उनके पवित्र अभ्यागमन की स्मृति में वहाँ माता मरियम की एक प्रतिमा है। स्वामी जी ने सुप्रसिद्ध जल में पुण्य स्नान किया और तत्पश्चात् जर्मनी को और बाद में स्विट्ज़रलैण्ड को प्रस्थान किया।
स्वामी जी १५ दिसम्बर को ज़्यूरिक से प्रस्थान कर असीसी की पवित्र भूमि की तीर्थयात्रा को गये जहाँ लगभग १८०० वर्ष पूर्व सन्त फ्रांसिस का जन्म हुआ था। जैसा कि इससे पूर्वतर बतलाया जा चुका है कि स्वामी जी अपने बालकपन से ही सन्त फ्रांसिस के जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे और उनके अपने जीवन की तुलना इस महान् ईसाई सन्त के जीवन से युक्तियुक्त रूप से की जा सकती है। वस्तुतः पाश्चात्य देशों में कुछ श्रद्धालु जन इन्हें भारत का सन्त फ्रांसिस मानते हैं। उन्होंने इस महान् सन्त की जन्मभूमि के दर्शन करने को अपना एक पुण्य सद्भाग्य माना और उस पावन केन्द्र में अपने को पवित्रीभूत अनुभव किया। तत्पश्चात् वह पैड्रेपियो को एक बार पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सैन गियोवन्नी रोटोण्डो गये।
उसके बाद स्वामी जी यरुशलेम तथा बेतलहम'[12] की पुण्य भूमि में गये जहाँ उन्होंने २५ दिसम्बर १९६१ को पवित्र ख्रीस्त-जन्मोत्सव मनाया तथा पाश्चात्य देशों के उनके बच्चों में अपना नियत कार्य पूर्ण करने के लिए मुक्तिदाता प्रभु को धन्यवाद दिया।
स्वामी जी की पश्चिमी गोलार्ध की प्रथम यात्रा समाप्त हुई। वह यरुशलेम से केयरो गये और वहाँ से वायुयान द्वारा १९६१ के अन्तिम दिनों में भारत आये। वह ३० दिसम्बर को मुम्बई पहुँचे और अल्पकालिक विश्राम के लिए कुछ समय के लिए दक्षिण भारत चले गये। वह २३ जनवरी १९६२ को आश्रम पहुँचे और सीधे श्री गुरुदेव के कुटीर में गये और उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
उनका सम्पूर्ण परिभ्रमण पूजनीय गुरुदेव स्वामी शिवानन्द तथा उनके दिव्य उद्देश्य की सेवा के रूप में था। दो वर्ष से अधिक समय पूर्व उन्होंने विदा लेने के रूप में पवित्र चरणों को स्पर्श किया था। कार्य समाप्त होने पर वह पुन: उन्हीं पवित्र चरणों की शरण में वापस आ गये। उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया था, उन्होंने जो कुछ भी सेवा की थी, उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया था, वह सब अब उन्होंने उन्हीं चरण-कमलों में विनम्रतापूर्वक समर्पित कर दिया।
षष्ठ अध्याय
विश्व-यात्रा पर
"उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।
-उदारचेता महानुभावों के लिए तो यह समस्त संसार ही उनका परिवार है" (नीति-शतक)।
गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात् स्वामी जी को गुरुदेव द्वारा अपने पीछे छोड़े गये विशिष्ट शिष्य-समूह के प्रमुख होने के नाते आश्रम का संचालन करना पड़ा। उन्हें व्यवस्था का विवरण देखने, महाद्वीपों में फैली हुई संस्था की बहुसख्यक शाखाओं से निकट सम्पर्क रखने तथा बहुत बड़ी संख्या में विशेष भक्तों की प्रार्थनाओं पर ध्यान देने के साथ-ही-साथ भूमण्डल के सभी कोनों तक दिव्य सन्देश पहुँचाना था। समग्र विश्वभर के भक्तों की प्रार्थनाएँ इतनी आग्रही थीं कि पहले से वहन किये दुर्वह उत्तरदायित्वों के होते हुए भी उन्हें उनके निमन्त्रण पर अनुक्रिया करनी पड़ी तथा उनकी प्रेममयी माँगों को पूरा करने के लिए विदेश जाना पड़ा। गुरुदेव शिवानन्द ने उन्हें अपना अवाशेष्ट जीवन लोक-संग्रहार्थ समर्पित करने के लिए आदेश दे रखा था तथा स्वामी जी सामान्य मानव-जाति की इस उत्कृष्ट आध्यात्मिक सेवा का भार अपने ऊपर लेने को सर्वथा तैयार थे।
श्रीलंका के भक्तों को ही उन्हें भारत से बाहर लाने में प्रथम सफलता प्राप्त हुई। उन्हें उनके दिव्य सम्पर्क का अनुभव पहले ही हो चुका था जब वह वहाँ सन् १९५० में गुरुदेव के साथ गये थे। तभी से ही वे उनके ऐसे ही एक अन्य अभ्यागम के लिए दिव्य जीवन संघ के प्रमुखालय से अनुरोध करते रहे थे। पन्दरह वर्ष बाद उन्हें स्वामी जी का अपने मध्य में स्वागत करने तथा उनकी ज्ञानमयी वाणी सुनने का असाधारण सुयोग प्राप्त हुआ। श्रीलंका में गुरुदेव के भक्त अब भी १३ जून १९६५ के उस रविवार को बड़ी ही भावुकता तथा श्रद्धा से स्मरण करते हैं; क्योंकि यह वही दिन था जब स्वामी चिदानन्द जी महाराज ने दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका की भूमि पर अपने पाँव रखे थे। रत्नालम हवाई पत्तन पर पहुँचने पर अन्य लोगों के अतिरिक्त स्वामी सच्चिदानन्द, वी. एफ. गुणरत्ने, एम. शिवरस तथा स्वामी शिवानन्द सच्चिदानन्द माता जी ने इनका सादर स्वागत किया। स्वामी जी के अभ्यागम ने जो गम्भीर धर्मोत्साह तथा पवित्र प्रत्याशा उत्पन्न की, दिन के समय स्वागत-समिति के अध्यक्ष ने इनका औपचारिक स्वागत करते हुए जो अर्थगर्भित शब्द कहे थे, उनसे वह सहज ही जानी जा सकती है। उन्होंने सादर उद्घोष किया : "इसी प्रकार एक दिन श्रद्धेय महेन्द्र थेरा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका की भूमि में पदार्पण किया था।" उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया कि जब आधुनिक श्रीलंका के आध्यात्मिक जागरण का इतिहास लिखा जायेगा तब स्वामी जी का दिव्य जीवन का सन्देश स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा।
कोलम्बो पहुँचने पर स्वामी जी का जनसंकुलित नागरिक-अभिनन्दन किया गया। कोलम्बो के महापौर विन्सेन्ट परेरा ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि उनके मध्य स्वामी जी की उपस्थिति से देश के सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक वातावरण में गम्भीर परिवर्तन घटित होगा। अभिनन्दन के उत्तर में स्वामी जी ने प्रथम तो कुछ स्तोत्रों का पाठ किया और तत्पश्चात् वह एक भावोद्दीपक भाषण देते रहे। उन्होंने अपने भाषण के उपसंहार में श्रोताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा : "हे मानव! सत्य को असत्य द्वारा अवगुण्ठित न होने दें, छिपाने न दें। सत्य को असत्य के आच्छादित करने वाले अन्धकार में लुप्त न होने दें। ज्ञान की प्रभा को अज्ञान के मेघों से आवृत्त न होने दें। इस तुच्छ सत्ता द्वारा, इहलौकिक क्षणिक जीवन द्वारा, जन्म-मरण-शील जीवन द्वारा अपने को पर।भूत तथा अभिभूत न होने दें, उसे आपसे अपने सच्चे ज्ञान को, अपने जन्मसिद्ध अधिकार को, अपने अमर स्वरूप की चेतना तथा अभिज्ञा को अपहरण करने न दें। आप अमर हैं। आप नित्य आत्मा हैं, जन्म-मृत्यु रहित हैं; अज, अमर्त्य तथा अविनाशी हैं। आप नित्य देदीप्यमान सत्ता हैं, अनादि-अनन्त दिव्य प्रकाश के दिव्य अंशु हैं।"
अपने एक सप्ताह के अल्पकालिक आवास-काल में स्वामी जी कोलम्बो, जाफना, चुन्नकम, ट्रिक्कोमाली, बट्टीकोला, कुरुनेगला, कैन्डी, श्रीलंका विश्वविद्यालय पेराडेनिया, नवलपीटिया तथा कटारगामा गये। इन सभी स्थानों में उनका भारी स्वागत हुआ तथा उन्होंने स्मरणीय आध्यात्मिक आबन्धों को पूरा किया।
जाफना नगर-भवन के एक सार्वजनिक स्वागत-समारोह में उनका भाषण विशेष रूप से आश्चर्यकर था। उन्होंने हार्दिक प्रार्थना से आरम्भ किया : "हे प्रभु! मैं अपने जीवन की सभी प्रवृत्तियों को, शरीर के सभी कर्मों को, हृदय के भावों को, मन के विचारों को, अन्तरतम अन्तर्जात प्रकृति की गति को, जीवन की सभी प्रवृत्तियों तथा गतियों को अपनी श्रद्धामयी पूजा के रूप में आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। जो-कुछ भी मैं बोलता हूँ, जो कुछ भी मैं करता हूँ, वह सब मैं अपनी श्रद्धामयी पूजा, आराधना, प्रेम तथा समर्पण के रूप में आपको अर्पित करता हूँ। इसे आप अपनी कृपा तथा अनुकम्पा से स्वीकार करें।" उसके पश्चात् दिया गया उनका भाषण भी उस समय जाफना के नागरिक के रूप में उनके समक्ष प्रकट प्रभु की प्रार्थना तथा उनके चरणों में विनम्र सेवा की उसी भावना से अधिभारित था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य भगवान् ही होना चाहिए तथा सत्य, शुचिता, विश्व-प्रेम तथा करुणा का सम्पोषण ही भगवत्पथ है। उन्होंने उन सबको भगवान् को सदा स्मरण करते रहने का परामर्श दिया और बताया कि समस्त प्रवृत्तियों के मध्य भी (भगवान् से) संसर्ग का भाव बनाये रखा जा सकता है। उन्होंने उन्हें दिनभर समय-समय पर मौन जप करने का स्वभाव डालने तथा कर्म को प्रभु की भेंट के रूप में करने का परामर्श दिया। उन्होंने अपने भाषण का समापन इस उत्कट अनुरोध के साथ किया : "मेरे प्रिय जाफना के नागरिको ! मेरे प्रिय ज्योतिर्मय अमर आत्माओ ! भगवान् की ओर अग्रसर होने के लिए जीवन-यापन करें। सद्गुण का पालन करने के लिए जीवन-यापन करें। अपनी अन्तस्थित दिव्य प्रकृति को प्रसारित तथा अभिव्यक्त करने के लिए जीवन-यापन करें। यही जीवन का अर्थ है। यही जीवन का उद्देश्य है। इसी में जीवन की सार्थकता है। यही आपका जीवन-लक्ष्य है।" उनके भाषण ने कुतूहली श्रोताओं तक के ऊपर जो आश्चर्यकर प्रभाव डाला उसे वहाँ पर उस समय उपस्थित लोग आज भी स्मरण करते हैं। तदनन्तर स्वामी जी जब चुन्नकम के शिव-मन्दिर में गये तो वहाँ उनका शानदार स्वागत करने के लिए उत्सुक लोगों की अभूतपूर्व भीड़ थी।
गुरुदेव शिवानन्द के भक्तों के लिए यह अभ्यागम और भी स्मरणीय था; क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि चिदानन्द के देहबन्ध में स्वयं गुरुदेव ही उनके पास पधारे हैं। नित्यलक्ष्मी ताम्ब्रीराजा नामक एक पुरानी भक्त ने, जो गुरुदेव से सन् १९४० से परिचित थी, अनुभव किया कि सन् १९६५ में जब स्वामी जी कुरुनेगला में उसके निवास स्थान पर पधारे, वह उनसे अन्ततः एकाकार हो गयी है। उसने घोषित किया: "अब सांसारिक जीवन से मेरा पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद हो गया है।" जब स्वामी जी कैन्डी पहुँचे तो योगिराज स्वामी सच्चिदानन्द जी तथा श्री सौली मारलाडे के नेतृत्व में वहाँ के भक्तों ने उनका सविनय स्वागत किया तथा उनके सम्मान में प्रशस्ति-पत्र भेंट किया। अपने उत्तर में स्वामी जी ने शिष्टतापूर्वक कहा कि एक सन्त एकमात्र भगवान् के गुणगान के लिए ही जीता है। सम्मान को तो उसे किंचिन्मात्र भी पसन्द नहीं करना चाहिए। अत्यन्त विनम्रतापूर्वक उन्होंने आगे कहा कि जिनकी आत्मा में वह निवास करते हैं और वह जो-कुछ जानते हैं, उसे जिनके चरणों में बैठ कर सीखा है, उन अपने गुरुदेव की तुलना में वह कुछ भी नहीं हैं। तत्पश्चात् उन्होंने भगवान् की खोज के विषय में अपनी ज्ञान-गिरा की वृष्टि की।
श्रीलंका की उनकी यात्रा के समय विभिन्न सम्प्रदायों तथा मतों के लोगों ने उनके प्रति समान सम्मान तथा स्नेह प्रदर्शित किया। सिद्धान्ती, वेदान्ती, बौद्ध तथा ईसाई सभी ने समान रूप से महाराजश्री पर अपने प्रेम तथा श्रद्धा की वृष्टि की। अपनी ओर से स्वामी जी समान भक्ति के साथ सभी गिरजाघरों, मन्दिरों तथा बौद्ध विहारों के दर्शन करने गये तथा उन सभी स्थानों में उन्होंने भगवान् की पूजा की। उन सभी लोगों का बहुमत-मतैक्य ह था कि वह जिन लोगों से मिलते, उन सबमें वह महान् ईश्वर-निष्ठा तथा बल अनुप्राणित करते थे। लोग उन्हें आश्चर्य तथा आदर से देखते और बुदबुदाते : "यह वह ईश-मानव है जो अपने उपदेशों का प्रचार करने की अपेक्षा उन्हें अपने जीवन में उतारता अधिक है।" विमल तपस्या की दीप्ति विकीर्ण करने वाला स्वामी जी का व्यक्तित्व मनोहर तथा अप्रतिहत था। श्रीलंका के एक विख्यात जिज्ञासु भक्त पादुका ने ठीक ही कहा था : "हम इस महात्मा के प्रीतिकर तथा कोमल आकार तथा रंग-रूप में अपने जीवन-व्रत के पवित्र उद्देश्य का निश्चय, लौह-मनस्क तथा सैनिकवत् आध्यात्मिक अनुशासन, किसी भी कुत्सित, अशोभन अथवा अधम विषय के प्रति तीव्र घृणा तथा सर्वाधिक उनकी विनम्रता, सत्यशीलता तथा विशद निष्कपटता पाते हैं-वास्तव में, उनके अनेक प्रशंसकों द्वारा उनके शिर पर प्रेमपूर्वक अनेक बार रखा गया प्रतिष्ठा तथा गौरव का किरीट कभी भी क्षण मात्र भी उनके शिर पर टिक नहीं सका; क्योंकि उनका शिर गुरुतर जीवन-दर्शन से बोझिल तथा अवनत था और किरीट को धारण करने के लिए कभी भी अनम्य तथा अहम्मन्य न था।"
स्वामी जी ने एक रोमांचक तथा स्फुरणकारी विदायी के सत्संग के साथ २२ जून को श्रीलंका से प्रस्थान किया। आठवें दशक में वह तीन विभिन्न अवसरों पर श्रीलका गये तथा प्रत्येक बार ही उन्होंने श्रीलंका की मनोरम भूमि में जनता को आध्यात्मिक उद्बोधन के लिए नव-प्रेरणा प्रदान की। आज वहाँ ऐसे असंख्य जिज्ञासु हैं जिन्होंने उन अभ्यागमों में से किसी-न-किसी को अपने हृदय में सँजोये रखा है जिन्होंने वहाँ अपनी अमिट छाप छोड़ी है।
श्रीलंका की यात्रा के एक वर्ष पश्चात् स्वामी जी पुनः आश्रम से बाहर-इस बार मलेशिया के भ्रमण के लिए-निकले। बंगाल की खाड़ी के उस पार के इस देश में गुरुदेव के प्रतिनिधि स्वामी प्रणवानन्द पहाराज जी मलेशिया की यात्रा के लिए महाराजश्री से अनुरोध कर रहे थे। सन् १९६६ में पुनः उनका स्नेहमय निमन्त्रण प्राप्त करने पर स्वामी जी ने हिमालय से मलाया की यात्रा की तथा वह वसन्त ऋतु में वहाँ बीस दिन रहे। मलाया देश में ही प्राचीन काल में गुरुदेव ने अनेक निर्धनों तथा रोगियों को सान्त्वना प्रदान करते हुए एक चिकित्सक के रूप में सेवा की थी। अत: स्वामी जी ने अपनी इस यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा न कह कर तीर्थयात्रा का विशेषण दिया। उन्होंने ५ अप्रैल को वायुयान द्वारा दिल्ली से प्रस्थान किया और उसी दिन सायंकाल को वह क्वेलालम्पुर पहुँच गये। इस यात्रा का तात्कालिक प्रकट उद्देश्य शिवानन्दाश्रम वातूगुहा में गुरुदेव की संगमरमर की प्रतिमा का अनावरण करना था। उन्होंने यह शुभग कार्य ९ अप्रैल को श्रद्धास्पद मनोभाव तथा अत्यधिक आनन्दबोध के साथ सम्पन्न किया। उन्होंने विशाल जनसमूह के मध्य में गुरुदेव की प्रतिमा के प्रतिष्ठापन की विधि सम्पन्न की तथा सम्यक् पूजा तथा भगवद्दर्शन के रहस्य पर प्रवचन किया। उसके पश्चात् वह इस देश की दिव्य जीवन संघ की विभिन्न शाखाओं को देखने गये। मलेशिया की रुचि तथा धर्म-वैविध्य वाली जनता इस यशस्वी अतिथि के प्रति उत्साह तथा भक्ति के साथ अनुक्रिया करने में अनन्य थी। वी. टी. साम्बनाथम तथा मणिकवासगम जैसे मलेशिया के राजनयिक स्वामी जी के वैश्व प्रेम तथा विश्वजनीन दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपने अभ्यागम से वहाँ जो उत्थान किया वह परवर्ती वर्षों में उन्हें उस देश में पुनः पुनः खींच ले जाने का कारण बना।
स्वामी जी मलेशिया से हांगकांग गये जहाँ वह एक सप्ताह से अधिक समय तक सत्संग कराते रहे और सन् १९६६ की ग्रीष्म ऋतु में आश्रम वापस आ गये।
अब स्वामी जी ने निश्चय कर लिया कि वह अभी भविष्य में कुछ समय तक विदेश की और अधिक यात्रा का अनुरोध स्वीकार नहीं करेंगे। वह लगभग दो वर्ष तक आश्रम तथा संस्था की देखभाल करने में व्यस्त रहे। किन्तु विश्व के विभिन्न देशों से प्रार्थनामय पत्रों की उनकी मेज पर वृष्टि होती रहती थी जिनमें भूभण्डल के विभिन्न भागों के उन सुदूर स्थानों में उनकी निजी यात्रा के लिए साग्रह अनुरोध होते थे। भारत के भीतर के भी भक्त उनके दर्शन करने तथा दिव्य उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। किन्तु इस भागवत पुरुष के पास बिलकुल समय न था। आश्रम को उनकी उपस्थिति की आवश्यकता थी, भारतवर्ष के भक्त भी उनके दर्शन के लिए लालायित थे तथा विश्वभर के शिवानन्द योग-वेदान्त-केन्दों के सच्चे जिज्ञासु सीधे उनके मुख से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने की याचना कर रहे थे। किन्तु चिदानन्द एक ही थे, तथापि उस एक ही रूप में अब इस प्रकार कार्य करने का निश्चय कर लिया मानो अनेक हों। कुछ भी हो, स्वामी जी ने सभी दिशाओं से आये हुए अत्यावश्यक निमन्त्रणों को समर्पण तथा सेवा की भावना से स्वीकार करने का निश्चय कर लिया। दक्षिणी अफ्रीका दिव्य जीवन संघ के मठाधीश डर्बन के स्वामी सहजानन्द की स्वामी जी से दक्षिणी अफ्रीका आने की आग्रहपूर्ण प्रार्थना पर विषय ने निश्चित रूप धारण किया। स्वामी जी ने समाधि-मन्दिर में गुरुदेव की पादुका-पूजा की तथा विदेश में दिव्य कार्य के सम्पादन के लिए आश्रम से प्रस्थान किया।
जिस दिन, २ मई १९६८ को स्वामी जी ने मुम्बई से समुद्र-यात्रा की, वह गुरुवार था। संयोगवश यह जगद्गुरु आदि शंकराचार्य का जन्म जयन्ती-दिवस भी था। स्वामी जी ने मुम्बई पोताश्रय के परिसर में ही एक विशेष आसन पर गुरुदेव की पादुका को रख कर गुरुओं के गुरु भगवान् दत्तात्रेय, जगद्गुरु शंकराचार्य तथा गुरुदेव शिवानन्द से उन्हें वहाँ विदा करने के लिए एकत्रित सभी भक्तों पर कृपा करने की प्रार्थना की तथा अपनी युगप्रवर्तक यात्रा आरम्भ की।
उन्होंने फ्रांसीसी पोत 'कैम्बोज' पर आरोहण किया तथा समुद्री मार्ग से मुम्बई से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा की। नैटाल पोर्ट (डर्बन पोताश्रय) में स्वामी सहजानन्द जी ने उनका स्वागत किया। पोत-घाट पर ही स्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना की, कुछ कीर्तन किया तथा एक संक्षिप्त भाषण दिया। इस भाँति विदेश में दिव्य सेवा का दीर्घकालिक दौर पुनः आरम्भ हुआ। वह डर्बन १० मई को पहुँचे तथा अगले दिन जोहानेसबर्ग के दिव्य जीवन संघ के सदस्यों को सम्बोधित किया जो वहाँ उन्हें प्रणाम करने के लिए आये हुए थे। १२ तारीख को उन्होंने शिवानन्द सण्डे स्कूल के नवयुवक छात्रों के समक्ष गुरुदेव के जीवन तथा शिक्षाओं पर प्रवचन किया।
इसी बीच डर्बन नगर उन्हें एक स्मरणीय नागरिक अभिनन्दन देने को तैयार था। १३ मई को डर्बन नगर-भवन में एक औपचारिक सभा में उमड़ती हुई विशाल भीड़ हिमालय के इस पुण्यात्मा सन्त का दर्शन करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। मोहक रूप से प्रसन्नचित्त तथा विनम्र, उन सभी लोगों के चिर सन्मित्रवत् व्यवहार करते हुए स्वामी जी ऊपर आये तथा विश्वविद्यालय कालेज, डर्बन के प्राचार्य प्रोफेसर एस. पी. ओलिवर से मिले जो उनके स्वागतार्थ वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रो. ओलिवर स्वामी जी को मंच पर लिवा ले गये तथा एक अन्ताराष्ट्रीय लब्धप्रतिष्ठ आध्यात्मिक प्रकाश-पुंज के रूप में उनका परिचय दिया। तत्पश्चात् उन्होंने स्वामी जी से श्रोताओं को अपना कुछ विशेष उपदेश देने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने अपने उन्नयनकारी भाषण में दिव्य जीवन की सारभूत बातों की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा बतलाया कि व्यक्ति अत्यधिक कार्य-समाकुल महानगर के मध्य में रहते हुए भी किस प्रकार दिव्य जीवन यापन कर सकता है। उन्होंने उन्हें दर्शाया कि किस प्रकार सच्ची सन्तता का जीवन तथा एक सामान्य व्यक्ति का दिन-प्रति-दिन का जीवन परस्पर विरोधी नहीं है; क्योंकि दिव्य जीवन मानव जीवन में व्याप्त दिव्य चेतना मात्र है।
प्रोफेसर ओलिवर स्वामी जी के व्यक्तित्व तथा भाषण से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी जी से विश्वविद्यालय कालेज, डर्बन में आने तथा अपने हृदय स्पर्शी शब्दों से छात्रों में प्रेरणा भरने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने इस निमन्त्रण को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। वह कालेज गये तथा छात्रों को सम्बोधित किया तथा बतलाया कि आत्मज्ञान की खोज क्योंकर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकती है और संकेत दिया कि यह ज्ञान केवल सरल तथा शुद्ध जीवन की अपेक्षा रखता है। इसी प्रकार शिक्षक-प्रशिक्षण-महाविद्यालय स्प्रिंगफील्ड में, जहाँ उन्हें उसके बाद आमन्त्रित किया गया था, स्वामी जी ने विद्यार्थी-जीवन में चरित्र के महत्त्व की चर्चा की तथा इस अपरिहार्य महत्त्वपूर्ण सत्य को अनेक सीधे-सादे उदाहरणों से समझाया। उन्होंने महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का विषय समाविष्ट करने के लिए एक परियोजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।
स्वामी जी १९६८ के शरत्काल तक दक्षिणी अफ्रीका में बहुकार्यसंकुल कार्यक्रमों में, देश को आड़े-तिरछे बार-बार पार करने में, मियर बैंक, नार्थडम्, स्टेंजर, डार्नल, आंझिटो, पीटर मेरीट्ज़बर्ग, रिचमाण्ड, जोहानेसबर्ग, प्रिट्रोरिया, लेनेशिया, ईस्ट लन्दन, पोर्ट एलिजाबेथ, किम्बर्ली, लेडी स्मिथ, केप टाउन आदि स्थानों को जाने में व्यस्त रहे। वह जहाँ-कहीं भी गये, वहाँ वह हिमालय के ऋषियों के उदात्त ज्ञान को सामान्य जनता को समझाने वाले साक्षात् दिव्य सन्देशवाहक प्रतीत हुए। उनके भाषणों की अपेक्षा उनका व्यक्तित्व सर्वत्र ही लोगों पर अपना जादू डालता-सा अधिक प्रतीत होता था। निश्चय ही यह विजय-यात्रा थी।
जब वह दक्षिणी अफ्रीका में इस भाँति योग तथा वेदान्त के सन्देश का प्रसार कर रहे थे, उस समय ही उन्हें अन्य अनेक देशों से निमन्त्रण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम उन्होंने स्वामी वेंकटेशानन्द का मारीशस आने का अनुरोध स्वीकार किया। वह वायुयान द्वारा उस द्वीप्य देश को गये तथा शिवानन्द योग-आश्रम की प्रतिष्ठित आधारशिला-रोपण-विधि का सूत्रपात किया। वह उस देश के विभिन्न भागों में अपने सन्देश का प्रसार करते हुए वहाँ एक सप्ताह रुके।
मारीशस के इस अल्पकालिक आवास के पश्चात् वह रोडेशिया गये तथा क्यू क्यू, सैलिसबरी तथा बुलवायो में अपने पवित्र सेवा-कार्य में प्रवृत्त रहे। वह मालवी (भूतपूर्व न्यासालैण्ड) की राजधानी ब्लैण्टायर भी गये। उसके पश्चात् एक भक्त जिज्ञासु उत्तम रणछोड़ के आग्रहपूर्ण तथा स्नेहमय आमन्त्रण पर उन्हें एक सप्ताह के कार्यक्रम पर जैम्बिया जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने लुसाका, लिविंगस्टोन, लुयान्श्या, मफिलियर, चिंगोला तथा न्डोला में जनता के समक्ष भाषण दिया।
स्वामी जी को न्डोला से मोम्बासा को प्रस्थान करना था। अब कीन्या में एक बहुत ही रोचक घटना हुई। उन्हें १७ नवम्बर को अपराह्न में मोम्बासा पहुँचना तथा उसी दिन सायंकाल को सार्वजनिक सभा में भाषण देना नियत था; किन्तु यह ज्ञात हुआ कि न्डोला से मोम्बासा के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। इसके लिए उन्हें दार-ए-सलाम जाना अपेक्षित था। ऐसा लगा कि मोम्बासा का कार्यक्रम निरस्त करना नहीं तो स्थगित करना अवश्यम्भावी है; किन्तु मोम्बासा में आयोजकों ने स्वामी जी के सायंकालीन कार्यक्रम का पहले से ही व्यापक प्रचार कर रखा था; अतः भक्तों के विशाल जनसमूह को दुःखद निराशा का सामना करना होता । इधर जब आयोजक प्रसन्नतापूर्वक अपनी तैयारी में लगे थे, उस समय तक स्वामी जी आकाश में ही थे और उनका वायुयान तंजानिया की राजधानी दार-ए-सलाम की ओर बढ़ रहा था। इतने में एक चमत्कार हुआ। वायुयान जब दार-ए-सलाम के हवाई पत्तन के ऊपर पहुँचा तो भू-नियन्त्रक ने विमान-चालक को यह कह कर उतरने की अनुमति देना अस्वीकार कर दिया कि हाल की वृष्टि से विमान-क्षेत्र अस्थायी रूप से असुरक्षित हो गया है। विमान-चालक को यहाँ के बदले मोम्बासा हवाई पत्तन जाने का निर्देश दिया गया। इस भाँति जैम्बिया की हवाई कम्पनी का जेट वायुयान आगे उड़ा और कीन्या के मोम्बासा हवाई पत्तन पर उतरा। मोम्बासा के भक्तों की प्रार्थना सुन ली गयी तथा अप्रत्याशित घटना घटी। स्वामी जी नियत समय पर कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए ठीक समय पर पहुँच गये मानो कि यह उड़ान इसी के लिए आयोजित की गयी थी। मोम्बासा में उतरने पर स्वामी जी ने भगवान् को धन्यवाद दिया और भक्तों से कहा : "गुरुदेव की कृपा की रहस्यमयी क्रियाशीलता अनेक प्रकार से अनेक अवसरों पर सर्वत्र जो अपने को अभिव्यक्त कर रही है, यह उनमें से एक है।"
स्वामी जी कीन्या तथा यूगाण्डा के विभिन्न भागों में दिव्य जीवन के सन्देश का प्रचार करते हुए नवम्बर के अन्त तक अफ्रीका महाद्वीप में ही इधर-उधर भ्रमण करते रहे। तदनन्तर उन्होंने रोम के मार्ग से पूर्वी अफ्रीका से पश्चिमी जर्मनी के लिए प्रस्थान किया। वह पोर्ज़ईल में लगभग एक मासार्ध तक श्रीमती तथा श्री हैन्स फ्रैंक के अतिथि के रूप में रहे। वहाँ अपना अस्थायी मुख्यालय स्थापित कर उन्होंने पश्चिमी जर्मनी के विभिन्न केन्द्रों का भ्रमण किया, अपनी चुम्बकीय मनोज्ञता से सैकड़ों व्यक्तियों को आकृष्ट किया तथा योग का सन्देश प्रसारित किया। वह सर्वप्रथम कोलोन गये जहाँ के समाचार-पत्रों ने इनके अभ्यागम का समाचार बड़े ही उत्साह से प्रकाशित किय।। राइन नदी के तट पर स्थित इस प्रख्यात औद्योगिक नगर से स्वामी जी एर्लेनगेन गये जो एक सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय-नगर है। यहाँ उन्होंने 'भगवत्प्राप्ति का मार्ग' विषय पर एक उन्नतकारी भाषण दिया। एर्लेनगेन से वापस आते समय उन्हें पता चला कि उनका विमान फ्रैंकफर्ट में उतरने को अनुसूचित है और फ्रैंकफर्ट से कोलोन के लिए उन्हें अपना विमान बदलना है। इससे उनका कोलोन का कार्यक्रम विपर्यस्त हो जाता; किन्तु जैसा कि पहले मोम्बासा में चमत्कार हुआ था, वैसा ही पुनः यहाँ हुआ। बहुत ही आश्चर्य में डालते हुए विमान ने कोलोन का सीधा मार्ग पकड़ा जिससे स्वामी जी के लिए सभा में ठीक समय पर सम्मिलित होना शक्य हुआ।
स्वामी जी पश्चिमी जर्मनी के इस यात्रा काल में शिवप्रेमानन्द माता के अतिथि के रूप में उनके शिवानन्द योग-स्कूल में दो बार डोरचौसेन गये। यहाँ पर उन्होंने विशिष्ट किन्तु विपुल श्रोताओं के सम्मुख सुव्यापक विषयसमूह पर शृंखलाबद्ध भाषण दिये जिनमें 'पश्चिम के लिए योग', 'गुरु का महत्त्व', 'योग की विश्वजनीनता', 'ध्यान' तथा गम्भीर आध्यात्मिक महत्त्व के ऐसे ही अन्य विषय थे। अनेक बहुश्रुत विद्वानों तथा धर्मनिष्ठ ईसाइयों ने आधुनिक काल के एक महायशस्क भागवत पुरुष के रूप में उनका अभिनन्दन किया। उनमें से कुछ लोगों को स्वामी जी का दर्शन करते समय अश्रुपात करते हुए देखा गया। उन्होंने अनुभव किया कि स्वामी जी ने अपना कुछ दिव्यानन्द उनमें अन्तरित कर दिया। उनके पवित्रता तथा प्रेम के परिमल से वे पुलकित थे। उन्होंने अनुभव किया कि स्वामी जी राम्बन्धी सबसे महत्तम चमत्कार स्वामी जी स्वयं हैं। आज भी वे अपने ऊपर स्वामी जी के गम्भीर प्रभाव की भावप्रवणता से चर्चा करते हैं और स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उनके जैसा व्यक्ति न तो उससे पूर्व और न उसके बाद में देखा है। एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी अपने वहाँ के आवास-काल में पादरियों तथा धर्मतत्त्वज्ञों के एक समूह से लम्बा विचार-विनिमय करते रहे। अन्त में जब वे विदा हुए तो उनमें से एक इतना अधिक प्रभावित हुआ कि स्वामी जी के कथन पर मन में गम्भीरता से विचार करने के लिए वह तत्काल जंगल में चला गया। वे ईसाई पुरोहित स्वामी जी से इतना अधिक प्रेम करते थे कि एक बार उन्होंने इस हिन्दू संन्यासी को एक अति-प्राचीन तथा प्रख्यात मठ में पवित्र भारतीय स्तोत्रों का पाठ करने के लिए आमन्त्रित किया। अतः स्वामी जी वहाँ गये। लगभग एक घण्टे तक उनके स्तोत्र-पाठ को श्रवण कर सारा मठ पुलकित हो उठा। स्वामी जी पोर्जईल में हैन्स फ्रैंक के अतिथि के रूप में रुके तथा 'योग तथा ख्रीस्तीयता', 'योग का स्पष्टीकरण', 'परिवार में योग', 'जीवन का स्वर्णिम काल' तथा 'योग सम्बन्धी तथ्य' विषयों पर अनेक भाषण दिये। तदनन्तर वह पोर्ज़ईल तीन बार गये तथा उन्होंने सैकड़ों जिज्ञासुओं को धारणा तथा ध्यानयोग अपनाने के लिए उत्प्रेरित किया।
सुप्रसिद्ध लेखक, पर्यटक तथा चित्रकार डा. लिली ई. स्मल्डर्स के निमन्त्रण पर स्वामी जी जर्मनी से ऐम्सटर्डम गये और वहाँ तीन सप्ताह ठहरे। ऐम्सटर्डम में स्वामी जी के कार्यक्रम आयोजित करने में माता पाल्स्ट्रा ने डा. स्मल्डर्स का साथ दिया। उनके अनुरोध पर स्वामी जी हालैण्ड की योग सोसायटी के दो केन्द्र देखने गये। वह अपने सहानुभूतिशील हृदय तथा आशा का सन्देश ले कर हिप्पियों के सामने भी गये। उनके पहुँचने के समय उनका क्लब-घर धुएँ से भरा था और उपद्रव का दृश्य था; किन्तु महाराजश्री के अभ्यागम पर वहाँ विलक्षण प्रशान्ति छा गयी तथा पथभ्रष्ट आत्माओं ने भी उनकी बातें श्रद्धामय सम्मान के साथ सुनीं। स्वामी जी ने भगवान् की इस स्वेच्छाचारी सन्तान की भी सेवा की और उनके उद्विकास के लिए उन्हें आवश्यक परामर्श दिया। इसके पश्चात् उन्होंने महाराजश्री के सत्संग के लिए फ्रांस, बेल्जियम तथा जर्मनी से विशेष रूप से आये हुए भक्तों के मध्य ख्रीस्त-जन्मोत्सव-सप्ताह व्यतीत किया।
लन्दन के हिन्दू-समाज के निमन्त्रण पर वह ख्रीस्त जयन्ती के पश्चात् वहाँ गये। लन्दन से वह श्री गाई डेस पिनार्डस के अतिथि के रूप में पैरिस गये जो आजकल 'शिवानन्द योग-वेदान्त-केन्द्र[13]' के नाम से पैरिस में दिव्य जीवन संघ की एक शाखा का संचालन करते हैं। श्री पिनार्डेस स्वामी जी तथा पोप की पारस्परिक भेंट की व्यवस्था करने को बहुत उत्सुक थे। उनके प्रयास से १९ फरवरी १९६९ को पोप पाल षष्ठ तथा स्वामी जी की एक अर्ध अशासकीय भेंट हुई। पोप इस भारतीय सन्त को देखते ही प्रेम से इतना भर गये कि उन्होंने परम धर्माध्यक्षीय प्राधिकार की प्रायिक औपचारिकताओं को अलग रख कर उनके हाथों को पकड़ लिया तथा उन्हें भाव-प्रवणता के साथ शिष्टाचार का आदान-प्रदान करते हुए देर तक पकड़े रखा। उन्होंने स्वामी जी का अभिवादन भारतीय रीति से किया तथा स्वामी जी ने उसके प्रत्युत्तर में पाश्चात्य लोकाचार के अनुसार गुरुदेव शिवानन्द के नाम में घुटने टेक कर उनका अभिवादन किया। पोप ने शिवानन्द का नाम सुनते ही सस्नेह गुनगुनाया: "मैंने आपके गुरुदेव के प्रशस्त आध्यात्मिक कार्य के विषय में सुना है। मैं आपके गुरुदेव के आध्यात्मिक कार्य को बहुत महत्त्व देता हूँ।" स्वामी जी ने पोप के प्रति अपने प्रेम तथा सम्मान के प्रतीक-रूप में गुरुदेव की पुस्तक 'Bliss Divine' (ब्लिस डिवाइन) उन्हें भेंट की। पोप ने भेंट को बड़ी ही प्रसन्नता से स्वीकार किया और आशा दी कि वह उसे रुचिपूर्वक पढ़ेंगे। वार्तालाप-काल
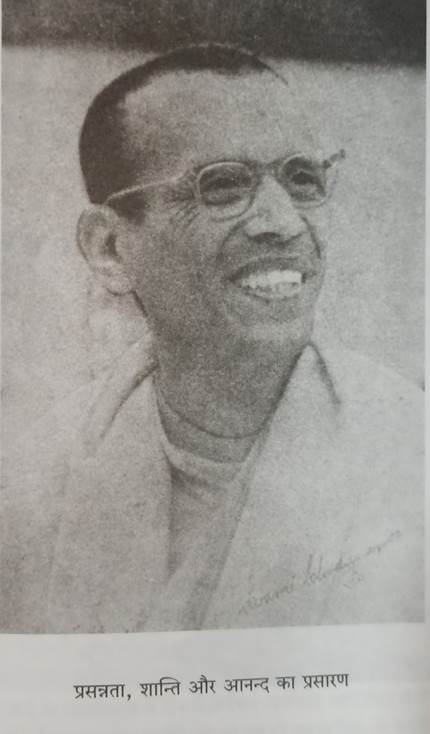

में उन्होंने बार-बार कहा : "मैं भारत को प्रेम करता हूँ। मैं भारत को प्रेम करता हूँ" तथा वार्ता के एक चरण में कहा: "भारत अलौकिक देश है। मैं एक बार पुन: भारत जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ।"" उन्होंने कहा कि वह उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो सत्य का साक्षात्कार कर लेने पर प्रेम-धर्म के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बाहर निकल आते हैं। स्वामी जी ने पोप को दिव्य जीवन संघ के प्रतिनिधि के रूप में शान्ति, प्रेम तथा आध्यात्मिकता के आदर्शों के प्रचार करने के अपने लक्ष्य के विषय में अवगत कराया और उनसे आशीर्वाद माँगा। पोप ने स्वामी जी को आशीर्वाद दिया और उनके पवित्र लक्ष्य में उनकी सफलता की कामना की। स्वामी जी ने अपने सुझावों का तैयार किया हुआ प्रारूप उन्हें दिया जिसमें कैथोलिक चर्च के तत्त्वावधान में रोम में सर्वधर्म-सम्मेलन आयोजित करने के लिए पोप से अनुरोध किया गया था। उन्होंने पोप को यह भी सुझाव दिया कि धार्मिक एकता का सन्देश पहुँचाने के लिए उन्हें एक विश्व-यात्रा आरम्भ करनी चाहिए। पोप ने सुझाब का प्रेमपूर्वक स्वागत किया और कहा : "मैं उसे ध्यानपूर्वक देखूँगा ।" उन्होंने उनके प्रेम के प्रतिदान में स्वामी जी को एक स्मारक-पदक प्रदान किया। वहाँ पर जो कतिपय व्यक्ति उपस्थित थे, उन्हें स्पष्ट हो गया कि ख्रीस्त-जगत् के परमधर्माध्यक्ष स्वामी जी के आध्यात्मिक व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे।
स्वामी जी रोम से एक सप्ताह के कार्यक्रम पर अथेन्स गये। अपने यूनान के यात्रा-काल में वह ग्रीक आर्थोडाक्स चर्च के मठवासियों से मिले जो एथोस पर्वत पर भव्य एकाकीपन में रहते थे। केवल मठवासी ही वहाँ ठहरते हैं, अन्य कोई भी नहीं ठहरता । वे सामान्यतया बाह्य जगत् से कोई भी सम्पर्क नहीं रखते हैं; किन्तु वे भी स्वामी जी से मिल कर तथा यूनानी दुभाषियों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का आदान-प्रदान कर अत्यधिक प्रसन्न हुए। स्वामी जी वहाँ दो मठों में रुके जो लगभग एक सहस्र वर्ष प्राचीन थे।
स्वामी जी १९६९ के अप्रैल माह तक एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के बहुसंख्यक देशों में भ्रमण कर चुके थे। तत्पश्चात् उन्होंने एटलांटिक महासागर पार कर 'प्रतीकवाद तथा यथार्थवादिता', 'मोक्ष तथा मन', 'भक्तिमार्ग', 'कर्म तथा प्राकृतिक नियम', 'योगे-मनोविज्ञान', 'मन्त्र', 'ध्यान', 'रहस्यात्मक अनुभव' आदि विषयों पर अपने कुछ सर्वाधिक रोचक भाषण देते हुए अक्तूबर तक अमरीका तथा कनाडा की यात्रा की। उन्होंने न्यूयार्क, वैन्कूवर तथा वाल्मोरिन में शृंखलाबद्ध भाषण दिये। इसी अवधि में उन्होंने ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय में 'मनुष्य, ध्यान तथा मोक्ष' विषय पर भाषण दिया। उन्होंने लारेन्टियन पर्वत के मध्य में 'अवितथ विश्व व्यवस्था' के सम्मेलन का उद्घाटन भी किया तथा वाल्मोरिन के योग-वर्ग के छात्रों में शृंखलाबद्ध भाषण दिया।
तत्पश्चात् उन्होंने दक्षिणी गोलार्ध की यात्रा की। वह दक्षिणी अमरीका गये जहाँ सैन्टियागो डि चिली, ब्यूनस आयर्स आदि नगरों में भाषण देते हुए अक्तूबर से वर्ष के अन्त तक रुके। माण्टेवीडियो में उनका पुजारियों की एक वादसभा में दूरदर्शन पर कार्यक्रम था। उन लोगों ने आध्यात्मिक विषयों पर कई परीक्षक प्रश्न पूछे। यहाँ पर अन्य अनेक उद्घाटनकारी बातों में स्वामी जी ने एक बात यह बतलायी कि किस प्रकार एक भी आसन अथवा प्राणायाम न करने पर भी व्यक्ति सच्चा योगी हो सकता है। उनकी यह मान्यता है कि योग केवल मनोभौतिक विज्ञान नहीं है।
स्वामी जी तदनन्तर ट्रिनीडाड तथा टोबैगो के दिव्य जीवन संघ के प्रमुख स्वामी सच्चिदानन्द के प्रेममय निमन्त्रण पर वेस्टइण्डीज़ गये। यहाँ उनका एक सप्ताह का बहुत ही कार्य-संकुल कार्यक्रम था। उन्होंने विवेकानन्द सांस्कृतिक वर्ग में 'धर्म का सार' पर, गोपी ट्रेस हिन्दू मन्दिर में 'सनातन धर्म' पर, चिदानन्द सांस्कृतिक केन्द्र में 'गुरुदेव का सन्देश' पर, पोर्ट आफ स्पेन हिन्दू मन्दिर में 'योग तथा स्वास्थ्य के लिए उसका महत्त्व' पर, गान्धी-आश्रम में 'धर्मों की मौलिक एकता' पर, सन्त केशवदास आश्रम में 'भक्ति तथा भगवन्नाम की महिमा' पर, शिवनारायण धर्मसभा में 'पूर्णता की ओर' पर, इन्टरप्राइज में 'दिव्य जीवन' पर, विश्व-हिन्दू-परिषद् में 'जीवन में महत्तम वस्तु' पर तथा माण्ड्रोज़ के वैदिक स्कूल में 'जीवन का वैदिक आदर्श' पर प्रवचन किये। उन्होंने जान एफ. कैनेडी मैदान में वेस्ट इन्डीज विश्वविद्यालय के छात्रों को भी सम्बोधित किया। उन्होंने स्वामी सच्चिदानन्द, ब्रह्मचारी कर्मानन्द तथा रामशरण मंगरू के सहयोग से चिदानन्द सांस्कृतिक केन्द्र की आधारशिला भी रखी। महाराज्यपाल सर सोलोमन होच्वाय, गृहमन्त्री गोराड मोन्टाहो, भारतीय उच्चायुक्त श्री रे, वेस्ट इण्डियन मामलों के मन्त्री श्री कमालुद्दीन मुहम्मद जैसे देश के प्रतिष्ठित राजनयिकों ने स्वामी जी से मिलने तथा उनके बोधप्रद भाषण सुनने में तीव्र रुचि प्रदर्शित की।
स्वामी जी अपने चौवनवें जन्मदिवस तक नयी दुनिया (अमरीका) में रहे। तत्पश्चात् वह वायुयान द्वारा फीजी गये। नन्दी हवाई पत्तन पर उनके पहुँचने पर स्थानीय रामकृष्ण सेवाश्रम केन्द्र के श्री स्वामी रुद्रानन्द जी महाराज तथा श्री आर. पी. गान्धी ने उनका स्वागत किया। फीजी में अपने दो सप्ताह के आवास-काल में उन्होंने प्राय: समूचे द्वीप की यात्रा की तथा लोगों को दिव्य जीवन-यापन करने को प्रेरित किया।
स्वामी जी फीजी से अनेक प्रतिश्रुत वचनों के पालन के लिए न्यूज़ीलैण्ड गये और वहाँ से उन्होंने आस्ट्रेलिया को प्रस्थान किया। वह १८ अक्तूबर को पर्थ पहुँचे । दिव्य जीवन संघ की पर्थ शाखा के अध्यक्ष डा. आर. जे. वर्थर[14] ने उनका स्वागत किया। स्वामी जी ने विज्ञान-भवन में अपनी अप्रतिम शैली में भाषण दिया तथा सैकड़ों जिज्ञासुओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। आस्ट्रेलिया के अपने आवास-काल में उन्होंने श्री वर्धर के आध्यात्मिक विकास से सन्तोष अनुभव किया तथा उन्हें स्वामी संगीतानन्द के नाम के साथ संन्यासाश्रम की दीक्षा दी। उन्होंने पर्थ, एडीलेड, सिडनी, ब्रिसबेन तथा कुछ अन्य स्थानों में अपने दिये हुए वायदों को पूरा करते हुए आस्ट्रेलिया में कुल तीन सप्ताह व्यतीत किये।
स्वामी जी एडीलेड के निकट आस्ट्रेलिया के योगी तथा श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के शिष्य चिरस्मरणीय श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी करुणानन्द के पास चार दिन रुके। करुणानन्द जी उन दिनों एडीलेड से कुछ मील बाहर एक वन्य कुटीर में रह रहे थे। वह उस समय दिव्य जीवन संघ की ओर से योग की एक हस्तमुद्रित मासिक पत्रिका निकालते थे। स्वामी चिदानन्द जी इस सदात्मा से मिल कर तथा उन्हें अपनी भावनाओं में भागीदार बना कर अत्यधिक प्रसन्न हुए। वह करुणानन्द जी को बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक व्यक्ति, साक्षात्कार-प्राप्त आत्मा मानते थे। करुणानन्द जी भी अपने प्रिय गुरुभाई स्वामी चिदानन्द जी के प्रति इसी प्रकार की श्रद्धा रखते थे। यवन्ने लेब्यू ने ठीक ही कहा : "उनको एक साथ देखना, उनके प्रेम को देखना एक अलौकिक, अविस्मणीय अनुभव था। करुणानन्द जब कभी चिदानन्द के विषय में कुछ कहते तो उनके मुखमण्डल से भक्ति विकिरण होती।" एडीलेड के निकट करुणानन्द के वन्य कुटीर में स्वामी जी का आवास स्मरणीय था; क्योंकि महात्माजनों के ऐसे मिलन में ईश्वरानुभूति उनकी वाणी तथा कार्य द्वारा अपने को अभिव्यक्त करती है।
आस्ट्रेलिया में स्वामी जी के आवास-काल में उनके सार्वजनिक तथा असार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले व्यक्तियों में से एक डा. विजयेन्द्र थे जो मुम्बई के अनुभवी योग-शिक्षक श्री योगेन्द्र के पुत्र हैं और मेलबोर्न विश्वविद्यालय में एक योग-केन्द्र का संचालन करते हैं तथा दूसरे व्यक्ति आस्ट्रेलिया में प्रख्यात योग-प्रचारक रोमा ब्लेयर (निर्मलानन्द) थे जिनका देशव्यापी योग-पाठ-कार्यक्रम चलता है।
अब स्वामी जी हिमालय की ओर वापसी यात्रा पर थे। पुराने वायदों को पूरा करने तथा अनेक स्थानों में भाषण देने में उन्होंने नवम्बर माह फिलीपाइन तथा हांगकांग में व्यतीत किया। तत्पश्चात् वह २४ नवम्बर को मलेशिया गये। जाफना की दिव्य जीवन संघ शाखा के नवनिर्मित प्रार्थना-भवन के उद्घाटन के लिए वहाँ अल्पकालिक निवास के पश्चात् वह मुम्बई आये जहाँ उनका शानदार स्वागत हुआ। वह २० दिसम्बर को दिल्ली पहुँचे। यहाँ उन्होंने स्वामी शिवानन्द सांस्कृतिक संघ में अपने सम्मान में आयोजित एक औपचारिक समारोह में राजधानी के नागरिकों को सम्बोधित किया। यही उनकी एक और अतिमहान् यात्रा की समाप्ति का सीमाचिह्न बना ।
स्वामी जी २२ दिसम्बर १९७० को आश्रम में वापस आ गये। आश्रमवासी तथा ऋषिकेश के भक्तजन, जो गत दो वर्षों से स्वामी जी की विश्व-यात्रा की अवधि में उनके द्वारा की जा रही स्मरणीय सेवाओं के विषय में बहुत-कुछ सुन रहे थे, उनके आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। आश्रम के प्रवेश-द्वार पर उनके पहुँचने पर कार्यकारी-अध्यक्ष स्वामी कृष्णानन्द जी ने सर्वप्रथम उन्हें माला पहनायी और उनके पवित्र चरणों में नतमस्तक हो बहुत ही हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया। स्वामी जी ने अपनी विशिष्ट नम्रता से इसका प्रतिदान दिया। उन्होंने कृष्णानन्द जी के चरण स्पर्श किये तथा उनका आलिंगन किया। स्वामी जी विशाल जनसमुदाय के मध्य से, जो उनके स्वागतार्थ वहाँ एकत्रित था, अकस्मात् आगे बढ़ते गये और चिरकाल के वियोग के पश्चात् अपनी माता से मिलने को उत्कण्ठित बालक की भाँति गुरुदेव के पवित्र समाधि-मन्दिर में चले गये। उन्होंने मौन रूप से गुरुदेव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, बाहर आ कर एकत्रित गुरुभाइयों तथा आश्रम-वासियों से कुछ मिनट तक बातें कीं और शान्ति से अन्दर जा कर अपना कार्य पुनः ऐसे आरम्भ कर दिया मानो कि वह एक-दो दिन ही अनुपस्थित रहे हों, मानो कि सद्यस्क अतीत में कुछ विशेष बात हुई ही न हो। अतः लोग जो उन्हें सच्चा स्थितप्रज्ञ कहने को प्रेरित होते हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
यह महती विश्व-यात्रा स्वामी जी की अन्तिम विदेश यात्रा नहीं थी। वह अपने प्रेमियों तथा भक्तों के दबाव से बारम्बार विदेश में जाते रहे हैं। इस भाँति उन्हें १९७२ में लेबनान, पश्चिमी जर्मनी तथा बर्लिन की एक माह की यात्रा करनी पड़ी। वह योग-शान्ति-निकेतन की माता शान्ता द्वारा आयोजित योग के छात्रों के एक प्रवर वर्ग में योगसूत्रों पर शृंखलाबद्ध व्याख्यान देने के एक विशेष कार्यक्रम से सन् १९७३ में पुनः बेरुत गये। सन् १९७५ में उन्हें योग-शिक्षक-सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वायुयान द्वारा बहामा द्वीप जाना पड़ा। वह संसार के विभिन्न भागों में वर्द्धमान महावीर का सन्देश पहुँचाने के लिए संघटित एक आध्यात्मिक शिष्ट-मण्डल में भी सम्मिलित हुए। उसी वर्ष उन्हें दिसम्बर माह में तीन सप्ताह के कार्यक्रम पर मलेशिया जाना पड़ा। सन् १९७६ के दिसम्बर माह में धर्म तथा शान्ति ने एशियाई सम्मेलन के प्रतिनिधियों में भाषण देने के लिए वह सिंगापुर गये। जोहान्सबर्ग'[15] के भक्तों का दीर्घकालिक अनुरोध उन्हें लम्बी अवधि के कार्यक्रम परवहाँ खींच ले गया। ऐसा हुआ कि दक्षिणी अफ्रीका तथा यूरोप के अनेक भागों की यात्रा करते हुए उन्हें नवम्बर ७७ से जून ७८ तक लगातार सात महीने की लम्बी अवधि व्यतीत करनी पड़ी। इस भाँति यह आगे चलता रहा है। अपने स्वास्थ्य तथा सुविधा से सर्वथा उदासीन रह कर यह करुणाशील व्यक्ति दूसरों के लिए और सदा ही उपयुक्त समय पर विश्व के विभिन्न भागों में मौके-बे-मौके एक संस्था अथवा समय से दूसरी संस्था अथवा समय को सदा स्थान-परिवर्तन करता रहता है।
स्वामी जी जहाँ-कहीं भी जाते, वहाँ वह स्वभावतः ही अपने को सुखी अनुभव करते। उदाहरणार्थ जब वह उमेगनी नदी के तट पर डर्बन में थे तो वह बड़ी उत्सुकता से वहाँ जाते तथा उसे दक्षिणी अफ्रीका की पावनी गंगा कहते थे। वह दिव्य जीवन के सप्राण मूर्तरूप में संसार में चारों ओर गये। यद्यपि लोग उन्हें एक महान् भागवत पुरुष कहते थे तथापि वह अपने आदिष्ट कार्य को, प्रेम के पवित्र सन्देशवाहक होने के कार्य को, ईश्वर के पितृत्व तथा मनुष्य के भ्रातृत्व के सन्देश को ले जाने के कार्य को करने वाले गुरुदेव के एक विनम्र सन्देशवाहक की तरह सदा व्यवहार करते थे। वह पश्चिम निवासियों को भारत के सनातन ज्ञान के भव्य उदाहरण तथा प्रेम और करुणा की मूर्ति, आधुनिक युग के यथार्थ सन्त फ्रांसिस प्रतीत हुए। यूरोप तथा अमरीका के जिज्ञासुओं तथा ज्ञानी लोगों ने, जो धनोपार्जन करने वाले योगियों अथवा अतीन्द्रिय शक्तियों वाले लोगों से ऊब गये थे, उन्हें परम प्रेम तथा श्रद्धा के योग्य गुरु समझा। इस आध्यात्मिक दोषदर्शिता तथा नित्य वर्धमान भौतिकवाद के अन्धकार-युग में भी अपने अपेक्षाकृत चरम रूप के वैज्ञानिक अविश्वास वाले विशेषकर पश्चिम के लोगों ने उनमें अविश्वसनीय रूप से दिव्यता का विशुद्ध तथा देदीप्यमान प्रकटीकरण पाया। उनकी आध्यात्मिक महत्ता को पूर्ण रूप से समझने के लिए किसी ने कभी भी परिचय के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं समझी। यह विशेष उल्लेखनीय है कि पश्चिम देशवासियों ने, जो भी उनसे मिले, उन्हें चमत्कार अथवा आशीर्वाद के खोटे आध्यात्मिक मापदण्ड से कभी नहीं मापा । वे उनके पास एक विरल वस्तु-दिव्यानन्द की सुस्पष्ट अनुभूति-के लिए बारम्बार जाते तथा उनकी भौतिक उपस्थिति के सान्निध्य मात्र से परम सन्तोष अनुभव करते।
स्वामी जी उद्विकास की सभी अवस्थाओं के लोगों के लिए आशा का सन्देश ले गये। स्वापकों के व्यसनी तथा कारागार की शलाकाओं के पीछे रहने वाले अपराधी भी उनकी उपस्थिति का उत्सुकता से स्वागत करते थे। सैन फ्रांसिस्को के एक कारागार में उनके दर्शन तथा वचनों ने दृढ़ीभूत अपराधियों के नेत्रों में आँसू ला दिये। उच्च कोटि के विवेकी लोगों ने भी उनकी उपस्थिति में अबोधता, आनन्द तथा उत्कर्ष की अलौकिक अवस्था अनुभव की है। ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टीना) की सारा हर्मन ने लिखा : "स्वामी चिदानन्द को हमसे विदा हुए कई वर्ष हो गये, किन्तु वह सदा हमारे हृदयों में निवास करते हैं। उन्होंने हमें और अधिक साधुवृत्त बनने की, अपने को पवित्र बनाने की आकांक्षा प्रदान की है। उनकी उपस्थिति ने ब्यूनस आयर्स में बहुत समुत्साह उत्पन्न किया। हमारे साथ उन्होंने जो दिन व्यतीत किये, उन दिनों में सभी उन्हें अपने पास रखना चाहते थे, सर्वत्र ही उन्होंने अपनी स्थायी स्मृति छोड़ी है। उनकी उपस्थिति सदा हमारे साथ है और उनका प्रकाश अब भी हमारे हृदय को प्रकाशित करता है।"
पश्चिमी देशों में उन्होंने जिज्ञासुओं के मन में यह बिठा दिया कि व्यक्ति के अपने ज्ञान के उपगमन में दूसरों का, संसार का तथा समाज का ज्ञान भी समाविष्ट है, इससे योग एक सर्वतोमुखी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता एक वैश्व संस्कृति है और इसकी प्राप्ति ही मानव जाति का चरम लक्ष्य है। उन्होंने बहुत ही सीधे-सादे ढंग से यह प्रमुख विचार सम्प्रेषित किया कि योग इस सर्वतोमुखी उपगमन का एक प्राविधिक नाम है। प्राचीन शास्त्रों के अपने निर्वचन में स्वामी जी ने जो उदार मनोवृत्ति, विश्वजनीन प्रेम तथा प्रज्ञा प्रदर्शित की, वह अपने-अपने मत तथा व्यवसाय का ध्यान न रख कर सभी को अच्छी लगने लगी। वह जब उद्यानों अथवा शाद्वल भूमि में विचरण करते तो अड़ोस-पड़ोस के लोग उनके मुख-मण्डल की दीप्ति देखने तथा उनके कार्य तथा चेष्टा की प्रत्येक मुद्रा में दिव्यता के प्राकट्य का अवलोकन करने को एकत्रित हो जाते थे। उन्होंने कभी भी अपनी सिद्धियाँ दिखलानी नहीं चाहीं। किन्तु इस ईशमानव की एक सामान्य-सी प्रार्थना अद्भुत कार्य कर सकती है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जब भूमण्डलभर के भक्तों ने साक्ष्य दिया है कि उनके आशीर्वादों ने लोगों की घोर विपत्ति से रक्षा की है। इन उदाहरणों में दस्यु के रिवाल्वर से ले कर असाध्य दूषण तक के पर्याप्त विविधता वाले अनुभव समाविष्ट हैं। कुछ लोगों ने तो सभामंचों पर भी इन अनुभवों का वर्णन करने का कष्ट उठाया है; क्योंकि वह जो अपनी उपस्थिति से पवित्रता, शुचिता तथा विनम्रता प्रसारित करते हैं, वही आध्यात्मिकत। की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभूति है। व्यक्ति लोगों को एक आलोचक के उस लहजे को प्रतिध्वनित करते हुए बारम्बार सुनता है जो उसने कहा : "वह जो कुछ भी उपदेश करते हैं, उसे हम उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए देखते हैं और ऐसा व्यक्ति संसार को हिला सकता है।"
स्वामी जी की ज्ञानमयी वाणी ने अनेक लोगों के जीवन में क्रान्ति ला दी है। माता सिमोनेटा डि सेसैरियो पैरिस के एक प्रसिद्ध भूषाचार-गृह में एक प्रमुख इतालवी अभिकल्पक थीं। स्वामी जी के एक भाषण ने, जिसे उन्होंने पैरिस में सुना, उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने भगवान् की खोज तथा मनुष्यों में निम्नतम की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। विलियम सी. ईलर्स एक समवाय (कम्पनी) के संचालक थे, किन्तु स्वामी जी के सम्पर्क ने उन्हें सहसा अन्तर्मुखी बना दिया और बहुत शीघ्र ही उन्होंने अपना जीवन उच्चतर कर्तव्य के लिए अर्पित कर दिया। इसी भाँति डान ब्रिडल, जो शान्ति-सेना के स्वयंसेवक थे, स्वामी जी के परिमल से आकर्षित हुए। पौला माता जेम्स टाउन में एक परिचारिका थीं। स्वामी जी के आशीर्वाद ने उनके जीवन की कायापलट कर दी।
उन्होंने भूमण्डल की सभी दिशाओं में शाश्वत सत्य का चिरन्तन सन्देश पहुँचाया तथा दर्शाया कि सभी धर्मों का उद्देश्य दिव्यता के स्तर तक मानवता का उत्थान करना है। उन्होंने नानाविध मतों के अनुयायियों से मनवा लिया कि योगमय जीवन का अर्थ है मानव-शरीर को व्याप्त करने वाला दिव्य जीवन। जहाँ-कहीं भी उन्होंने भाषण दिया, वहाँ उन्होंने लोगों के हृदय में गम्भीर प्रभाव डाला तथा उन मृण्मय मनुष्यों में से अनेकों को गतिशील आध्यात्मिक वीर में परिवर्तित कर उन्हें आध्यात्मिक जीवन का पथ अपनाने के लिए प्रेरित किया. जो इस प्रकार का साहसिक कार्य तत्काल आरम्भ करने की स्थिति में नहीं थे, वे कम-से-कम अपनी गहरी आत्म-निद्रा से जगा दिये गये हैं। वह दिग्भ्रान्त तथा अशान्त पाश्चात्य देशों के लोगों के लिए शान्ति तथा असम्भ्रम का आश्वासन ले गये। उन्होंने दर्शाया कि आध्यात्मिक प्रगति आधुनिक जीवन में व्यस्त कार्यक्रम के अनुकूल है तथा आध्यात्मिकता का सम्पोषण महानगरों के ठोस राजपथ पर उतना ही किया जा सकता है जितना कि हिमालय के विरलित शिखरों पर। क्षुद्र तथा हिंसात्मक प्रतिद्वन्द्विता से घिरे हुए समाज को उन्होंने अनात्मशंसा तथा आत्मत्याग की महिमा दिखलायी तथा लोगों में नव-विश्वास भरा, उनमें उच्चतर आत्ममय जीवन के नूतन आनन्द का संचार किया और इसे उन्होंने अपने उद्बोधक भाषणों तथा प्रेरक कीर्तनों से उतना ही किया जितना कि अपने सुन्दर उदाहरण से ।
सप्तम अध्याय
सन्तों की संगति में
"महत्संगस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च
-महात्माओं का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है" (नारदभक्तिसूत्र-३९) ।
स्वामी चिदानन्द ने दो दशकों तक विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण किया, बहुत बड़ी दूरी तय की तथा महाद्वीपों के आर-पार अपने यश की सुरभि फैलायी। उन पर अतुलनीय श्रद्धा तथा प्रशंसा की वृष्टि होती रही, बहुत बड़ी संख्या में नगर तथा लोग उनके दर्शन की माँग करते रहे, आध्यात्मिक तथा प्रापंचिक दोनों प्रकार के अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि तथा सकामनाएँ अर्पित कीं; किन्तु वह सदा की भाँति ही वही विनम्र तथा सरल सन्त, गुरुदेव का प्रकाश विकिरण करने वाले क्रकच (प्रिज्म; बने रहे। लोक-संग्रह तथा एकान्त-साधना के अतिरिक्त यदि उनकी कोई वैयक्तिक कामना थी तो वह थी सन्तों की संगति की। उनके मन में यह कभी नहीं आता है कि वह स्वयं एक उच्च कोटि के सन्त हैं जो अपने को किसी उत्कृष्ट एकान्तता में रखने का पर्याप्त कारण है। गुरुदेव ने बार-बार कहा था कि 'चिदानन्द एक जन्मजात सन्त, आदर्श योगी, परम भक्त तथा महान् ज्ञानी हैं' तथा इस दृढ़ोक्ति की सत्यता स्वामी जी के जीवन तथा कार्यों ने अनेक प्रकार से सिद्ध भी कर दी है। निष्कल्मष व्यक्तिगत पवित्रता तथा सजातीय मानवों के लिए गहरी संवेदना, जो उनके समग्र जीवन की विशिष्टताएँ हैं, किसी महान् सन्त में ही हो सकती हैं। एक ओर तो वह अपनी समस्त संवेदना तथा लोक-संग्रह को रखते हुए भी अपने हृदय के गुप्त प्रकोष्ठ में निरन्तर प्रतिष्ठित रहते हैं, अनादि तथा अमर सत्ता के साथ एकीभूत रहते हैं तो दूसरी ओर अपनी पूर्ण अनासक्ति तथा निरवशेष आत्म-तुष्टि के होते हुए भी वह सभी मतों तथा देशों के सन्तों से मिलने तथा उनके साथ संलाप करने को सदा लालायित रहते हैं। प्रवृत्ति के आन्तर तथा बाह्य क्षेत्रों में जैसा एकीकरण चिदानन्द लाते हैं वैसा केवल एक आदर्श योगी ही कर सकता है। उनके सदृश सरलता, विनम्रता तथा अपने चतुर्दिक् के सभी अस्थावर प्राणियों के प्रति प्रखर किन्तु अनासक्त प्रेम एक परम भक्त में ही हो सकता है। जीवन के गम्भीर दार्शनिक सत्यों के व्यक्तीकरण की उनकी सहजता तथा प्रशस्य सरलता केवल महान् ज्ञानी में ही हो सकती है। स्वामी जी कदाचित् ही कभी कोई उद्धरण देते हैं। उन्हें अपने भाषणों के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, उसे वह प्राय: अपने अन्दर से ही लाते हैं; तथापि वह अपने सभी धर्मोपदेशों में ऐसी अति-जटिल तथा दुर्बोध समस्याओं की चर्चा करते तथा उन्हें स्पष्ट करते रहते हैं जिससे प्रकाण्ड वेदान्ती भी विस्मित तथा अभिभूत हो जाते हैं। जब वह अपना मुँह खोलते हैं, तो वह सहज ज्ञानी की अवस्था में होते हैं। जब कभी वह बातें करते हैं तो उनके ओष्ठों से सुचारु रूप से विद्वत्ता मात्र नहीं अपितु ज्ञान टपकता है। ये बातें इतनी सुविदित हैं कि इनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। भूमण्डल के सभी सुदूर भूभागों में असंख्य कृतज्ञ साधकों ने स्वामी जी में भक्ति, ध्यान तथा ज्ञान के अद्भुत समन्वय के अपने-अपने मूल्यांकन अंकित किये हैं। यदि मानव जाति के सामान्य लोगों की ऐसी अनुक्रिया है तो प्रश्न उठता है कि उनके समान अवाप्ति वाले लोग उन्हें किस रूप में देखते हैं? स्वामी जी सन्तों तथा योगियों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं और वे लोग इनके साथ कैसा व्यवहार करते तथा इन्हें कैसा मानते हैं? सन्तों की रीति अबोधगम्य होती है, उनके सम्भाषण की भाषा हमारे लिए अत्यधिक गूढ़ तथा 7 रहस्यपूर्ण होती है। तथापि उनकी पारस्परिक अनुक्रियाएँ तथा समादर कभी-कभी ऊपर आते हैं और यह विचाराधीन पूतात्माओं की महत्ता को समझने का प्रयास करने = वाले व्यक्ति के लिए निश्चय ही परम महत्त्व का विषय है।
सन्तत्व स्वामी जी के जीवनभर उनके अप्रतिरोध्य आकर्षण का विषय रहा है। किन्तु यह सन्तत्व ऐसा नहीं था जो किसी विशेष वर्ग अथवा साधना के अन्तर्गत हो। सामान्य संन्यासी से भिन्न, स्वामी जी अपने जीवन के प्रारम्भिक काल से ही, जहाँ-कहीं भी उन्हें सन्तत्व दिखायी देता, उस पर ध्यान देने तथा उसको महत्त्व देने को पर्याप्त संवेदनशील थे। गैरिक वस्त्र उनके हृदय में प्रवेश पाने के लिए कोई आवश्यक पारपत्र न था। उदाहरणार्थ, गान्धी जी उनके लिए आजीवन एक महान् सन्त बने रहे। वह उन सर्वप्रथम सन्तों में से एक थे जो उनके जीवन में बहुत ही अल्पायु में आये तथा जिन्होंने उनके व्यक्तित्व पर अपना अमिट प्रभाव डाला। सत्य, अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य, बो बापू जी के सिद्धान्त थे, श्रीधर के प्रारम्भिक जीवन से ही उनके वैयक्तिक स्वीकृत धर्म बन गये। राम-नाम ने, जो गान्धी जी का प्रायः प्राण था, उनके हृदय में उसके समान स्थान पाया। वास्तव में, व्यक्ति स्वामी जी के जीवन में ऐसी अनेक महत्त्वपूर्ण बातें देख सकता है जिनमें उनके ऊपर गान्धी जी का प्रभाव अन्तर्भूत है। उदाहरणार्थ व्यक्ति इस दिशा में उनकी कुष्ठियों की सेवा तथा हरिजनों की पूजा की ओर इंगित कर सकता है।
अपनी हीरक जयन्ती के उत्सव-काल में गान्धी-जयन्ती के अवसर पर उन्होंने हरिजन-अतिथियों के चरणों में मूलार्थानुसार प्रणिपात कर तथा उनकी थालियों से प्रसाद माँग कर उनका जिस प्रकार आतिथ्य-सत्कार किया, उसे देख कर लोग सम्भ्रान्त तथा विस्मयाकुल हो गये। गुरुदेव शिवानन्द भी गान्धी जी के प्रति इसी प्रकार का सम्मान भाव रखते थे। वह अपने प्रेम के प्रतीक-रूप में उन्हें अपने सभी प्रकाशन भेजा करते थे। एक बार उन्होंने स्वामी जी को अपने वैयक्तिक प्रतिनिधि के रूप में योग पर अनेक नवीनतम पुस्तकों के साथ भेजा। सन् १९४६ को अत्युष्ण जून मास में स्वामी जी, जब वह गैरिक वस्त्ररहित एक अवर ब्रह्मचारी थे, रीडिंग रोड (अब मन्दिर-मार्ग) के उत्तरी छोर पर स्थित भंगी-बस्ती गये जहाँ महात्मा जी उन दिनों ठहरे हुए थे। जब वह पहुँचे तो दिन के ढाई बजे थे। भीषण ताप था। गान्धी जी उस समय एक कच्चे पर्णकुटीर में अपने शिर पर गीला तौलिया बाँधे हुए एक काष्ठ-फलक पर बैठे थे। शिवानन्दाश्रम के इस अवर ब्रह्मचारी को भारत के अनभिषिक्त सम्राट् के सम्मुख जब पहुँचाया गया, उस समय वह विश्राम कर रहे थे।
मानव-जाति के दो प्रबुद्ध सेवक सामान्य परिसर में मिले। स्वामी जी ने अपने मस्तक को बापू जी के चरणों में परम विनम्रता के साथ रख कर उन्हें नमस्कार किया। यह साधकों के लिए शिक्षाप्रद कार्य था जो प्रायः, जिन्होंने साधुवेशभूषा को धारण नहीं किया है, उनकी पात्रता का ध्यान किये बिना उनकी अपेक्षा स्वयं के वरिष्ठ होने की कुछ सूक्ष्म भावना से आचरण करते हैं। बापू जी ने गुरुदेव के सम्बन्ध में सस्नेह पूछताछ की तथा शिवानन्द जी महाराज की बहुमूल्य पुस्तकें समय-समय पर प्राप्त करते रहने पर अपनी कृतार्थता व्यक्त की। तत्पश्चात् स्वामी जी ने गुरुदेव की नवीनतम पुस्तकों का पुलिन्दा भेंट किया। गान्धी जी ने बड़े स्नेह से पुलिन्दा खोला तथा प्रत्येक पुस्तक पर आदर के साथ दृष्टिपात किया। वह दिव्य जीवन संघ की प्रवृत्तियों से परिचित थे। उन्होंने अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया। बापू जी से विदा लेने से पूर्व स्वामी जी ने उनका आशीर्वाद माँगा। गान्धी जी ने, जो जहाँ तक उनका सम्बन्ध है स्वामी जी की सन्तसुलभ महत्ता से प्रभावित हो चुके थे, कहा: "आप पहले से ही भाग्यशाली है। सर्वशक्तिमान् प्रभु आपको आपकी खोज में अपनी कृपा प्रदान करें!" जब स्वामी जी ने महात्मा जी से गुरुदेव के लिए सन्देश माँगा तो उन्होंने बड़ी ही नम्रता से उत्तर दिया : "मैं क्या सन्देश दे सकता हूँ? स्वामी जी का आध्यात्मिक जीवन का सन्देश विश्वभर में सहस्रों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। हमें ऐसे सत्कार्य की आवश्यकता है। कृपया उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा।" ऐसा कहते हुए गान्धी जी ने अभिवादन में अपने दोनों हाथ जोड़ लिये।
यह महात्मा जी के साथ स्वामी जी की द्वितीय तथा अन्तिम भेंट थी। इसमें अतीव आत्मीयता अथवा चमत्कारिता जैसा कुछ भी न था, तथापि यह स्वामी चिदानन्द की आजीवन अन्त: प्रेरणा बनी रही। गान्धी जी के प्रति स्वामी जी का प्रगाढ़ सम्मान निम्नांकित पंक्तियों से प्रकट होता है जिन्हें उन्होंने सन् १९६९ में गान्धी-शताब्दी-समारोह के अवसर पर कहा था : "यह वर्ष धन्य है जो इस वास्तविक महान् आत्मा के इस भूलोक में आगमन की शताब्दी को लक्षित करता है। यह गान्धी-वर्ष मेरे लिए वस्तुतः राम-नाम-वर्ष का, सत्यभाषण, वचन-पालन, आत्मपरीक्षा, उपवास, प्रार्थना तथा निस्स्वार्थ सेवा का वर्ष है। मेरे लिए इन सबका अर्थ गान्धी जी है।"
सन्तों की संगति में स्वामी जी का आचरण विशेष रूप से शिक्षाप्रद होता है। भारतीय परम्परा के पक्के अनुयायी वह वयोवृद्ध सन्तों को बड़ी ही विनम्रतापूर्वक नमस्कार करते, उनका अत्यधिक शिष्ट तथा अवधानपूर्ण रीति से आतिथ्य-सत्कार करते तथा उन्हें सम्मान देते हैं। गुरुदेव के जीवन काल में कैलास-आश्रम के महामण्डलेश्वर स्वामी विष्णुदेवानन्द जी महाराज, हिमालय के चूड़ामणि तथा आकाशदीप उत्तरकाशी के स्वामी तपोवन जी महाराज, गुरुदेव के पूर्वाश्रम के सहपाठी तथा दक्षिण भारत के सन्त-विद्वान् कवियोगी महर्षि शुद्धानन्द भारती जैसे वयोवृद्ध लब्धप्रतिष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति आश्रम में आया करते थे। उस समय स्वामी जी महासचिव थे। वह उन सबकी सेवा का सभी उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया करते थे और इसे अपनी लोकप्रसिद्ध विनम्रता से सम्पन्न करते थे। कवियोगी के मिलन को वह एक शताब्दी के सत्संग के तुल्य मानते थे। इसी भाँति वह वर्ष में न्यूनातिन्यून एक बार गुरुदेव की भेंट के साथ कैलास-आश्रम के महामण्डलेश्वर के दर्शन करने को उत्सुक रहते थे।
शिवानन्दाश्रम के अपने प्रारम्भिक आवास-काल में एक बार स्वामी जी अस्वस्थ हो गये। गुरुदेव ने हरिद्वार के एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक वैद्य की देख-रेख में उनके उपचार की व्यवस्था कर दी। स्वामी जी को वहाँ गुरुदेव के एक भक्त के पास रहना था। जब हरिद्वार में उनका उपचार चल रहा था, उस अवधि में वह स्वामी आत्मानन्द नामक सन्त के सम्पर्क में आये जो सुप्रसिद्ध स्वामी ब्रह्मानन्द के एक शिष्य थे। स्वामी आत्मानन्द पारस्परिक वार्तालाप-काल में साधक के जीवन के एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू पर बल दिया करते थे। वह इस बात की महती आवश्यकता मानते थे कि साधक को सांसारिक व्यक्तियों से अपने को दूर रखना चाहिए। यदि ज्ञानी जनों की संगति में रहना उसके लिए सम्भव न हो सके तो पूर्ण एकान्तवास करना उसके लिए श्रेयस्कर है। तथापि उनकी यह मान्यता थी कि ज्ञानी जनों की संगति साधक के लिए अत्यावश्यक है। स्वामी आत्मानन्द के सत्संग के महत्त्व पर बल देने से स्वामी जी के मन पर उसकी गहरी छाप पड़ी।
गुरुदेव जब कभी स्वामी जी को किसी काम से किसी अन्य स्थान को भेजते तो वह समीपवर्ती महात्माओं के दर्शन के सुअवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देते थे। एक बार स्वामी जी नेत्रों की जलन से पीड़ित थे। गुरुदेव ने उन्हें स्वर्गाश्रम जा कर आश्रम के औषधालय में अपने नेत्रों की जाँच कराने का परामर्श दिया। अतः स्वामी जी स्वर्गाश्रम गये। वहाँ उन्हें पता चला कि एक प्रबुद्ध आत्मा, परमहंस नारायण स्वामी उसी समय स्वर्गाश्रम में आये हैं। नारायण स्वामी अपने पूर्वाश्रम में एक न्यायाधीश थे। अपनी पचासवें वर्ष की आयु में उन्होंने स्वप्न में अपने गुरु के रूप में भगवान् नारायण का दर्शन किया। उन्होंने दूसरे दिन प्रातःकाल ही अपनी ऐश्वर्यशाली जीवन-वृत्ति को त्याग दिया तथा बदरीनाथ की यात्रा की जहाँ भगवान् नारायण मन्दिर के सामने उनके समक्ष प्रकट हुए। तत्पश्चात् वह भागवतीय चेतना में अहर्निश अभिनिविष्ट रह कर सदासर्वदा अपनी साधना में तल्लीन रहते। वह कभी नर्मदा तट पर वास करते तो अन्य समय पर उत्तरकाशी में। केवल मध्य शिशिर में ही वह स्वर्गाश्रम में कुछ दिनों तक रहा करते थे। उनके इस प्रकार के एक आगमन के समय ही स्वामी चिदानन्द जी की इस महान् तपस्वी से भेंट हुई और तत्पश्चात् वह इस महाभाग आत्मा के निकट सम्पर्क में आये। जब उन्होंने स्वर्गाश्रम में उस सन्त का दर्शन किया तो उन्हें मालूम हुआ कि सन्त की सम्पत्ति मात्र टाट की बोरी थी जिसका वह वस्त्र के रूप में उपयोग करते थे तथा एक हंस-दण्ड था जो उनके संन्यासाश्रम का चिह्न था। उस समय नारायण स्वामी पच्चीस वर्ष की दीर्घावधि तक चलने वाले अपने मौनव्रत को पूर्ण कर चुके थे। वह सत्यवादिता तथा वाणी की मधुरता पर विशेष बल देते थे। वह साधक के लिए आहार के उचित चयन की महती आवश्यकता बतलाते थे। अन्य विषय जिसको वह महत्व देते थे, वह था प्रतिदिन न्यूनातिन्यून ग्यारह माला (११८८ बार) अपने इष्ट-मन्त्र का अवश्यमेव जप । स्वामी जी ने उनमें विनम्रता तथा सरलता को मूर्तिमान पाया। यह मन्त केवल दूध तथा उबाले तथा घी में तले नमक-रहित आलू पर निर्वाह करते थे। स्वामी जी ने एक दिन प्रातःकाल उन्हें वन में नारायण के दिव्य नाम के जप में तल्लीन देखा। उनके आनन्दमय मुखमण्डल से स्वर्गिक आह्लाद फैल रहा था। स्वामी जी इस आनन्दमय अवस्था में उनका दर्शन लगातार घण्टों तक करते रहे और उन्होंने स्वयं भी उस एकाकीपन में अन्तरात्मा के आनन्द का अनुभव किया। स्वामी जी के लिए ऐसे सन्तों का संग उनके जीवनभर सदा ही एक स्मरणीय तथा सजीव अनुभव रहा है।
प्रतिष्ठित दिव्य व्यक्तियों के साथ स्वामी जी के सम्बन्ध की विशेषता वस्तुतः अवर्णनीय है। वर्तमान काल में आध्यात्मिक जगत् में श्री श्री माँ आनन्दमयी उच्च कोटि की दिव्य के रूप में दीप्तिमान हैं। उनके साथ स्वामी जी का सम्बन्ध तथा व्यवहार वास्तव में उन्नतकारी तथा रोमहर्षक है। वे दोनों परस्पर जो प्रेम तथा सम्मान प्रकट करते हैं उसकी गहनता सम्पर्क की एक वास्तविक दिव्य परिपाटी व्यक्त करती है। सन् १९४८ के मधुमास में पूज्य स्वामी जी ने वाराणसी में प्रथम बार श्रद्धास्पद माता जी का दर्शन किया। वह उस समय मेयो चिकित्सालय में दीर्घकालिक उपचार से स्वास्थ्य-लाभ के पश्चात् नागपुर से वापस आ रहे थे। शिवानन्दाश्रम की वापसी-यात्रा में वह वाराणसी में रुके तथा श्री माँ के पवित्र आश्रम में गये। श्री माँ उन दिनों एक गायत्री महायज्ञ करवा रही थीं तो तीन वर्ष तक चलता रहा। इस महायज्ञ-काल में ही दोनों दिव्य व्यक्ति परस्पर मिले। आठ वर्ष के अनन्तर जब श्री माँ गुरुदेव शिवानन्द से मिलने ऋषिकेश आयीं तो उन्हें एक बार पुनः उनके दिव्य सान्निध्य के आनन्दोपभोग का प्रशस्य अवसर प्राप्त हुआ।
गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात्, स्वामी जी तथा श्रद्धास्पद श्री माँ जी सत्संग के आनन्द हेतु अनेक बार परस्पर मिले। सन् १९६४ में जब गुरुदेव की जन्म-जयन्ती मनायी गयी तो पूजनीया माँ आनन्दमयी ने पुण्य-श्लोक गुरुदेव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपनी उपस्थिति से समारोह को सम्मानित किया। श्री माँ में स्वामी शिवानन्द जी तथा स्वामी चिदानन्द के लिए असाधारण प्रेम तथा सम्मान है। वह इन दोनों में कोई भेद नहीं करतीं। आज भी वह स्वामी जी को 'शिवानन्द बाबा' कह कर सम्बोधित करती हैं। वह चिदानन्द जी महाराज के लिए प्रशंसात्मक भावों से ओत-प्रोत हैं। उनका विचार है कि स्वामी जी की सामान्य चेष्टश भी ध्यान देने योग्य है। उन्हें ऐसा कहते हुए सुना गया : "स्वामी जी जब निश्चल बैठे होते हैं, उस समय भी उनका अंग-विन्यास एक बहुत ही सौम्य मुद्रा होता है।" वह उनको अपनी सन्तान के समान प्रेम करती हैं, योगी के रूप में उन्हें सम्मान देती हैं, सन्त के रूप में उनकी प्रशंसा करती हैं तथा अपने मित्र के समान उनके साथ व्यवहार करती हैं। इसी प्रकार स्वामी जी भी उन्हें भगवती माँ का अवतार मानते हैं।
श्री माँ सदा ही स्वामी जी को श्री आनन्दमयी संघ द्वारा समय-समय पर आयोजित संयम-सप्ताह-महाव्रत में सम्मिलित होने तथा उसमें भाग लेने वालों को सम्बोधित करने के लिए स्नेहमय निमन्त्रण देती हैं। स्वामी जी भारत के विभिन्न स्थानों में होने वाले इन समारोहों में, जब भी सम्भव हो पाता है, सम्मिलित होने का निश्चय रखते हैं। हाल में कोलकाता के निकट भाषा ग्राम में श्री माँ के भक्तों ने अहमदाबाद के निकट इसी प्रकार के एक समारोह में तीन दिन सम्मिलित होने के लिए स्वामी जी को आमन्त्रित किया। श्री माँ ने, जिनकी उपस्थिति में निमन्त्रण दिया गया, अपना मत व्यक्त किया कि बाबा के लिए तीन दिन अपर्याप्त होंगे और कम-से-कम पाँच दिन तक समारोह में उपस्थित रहने का उनसे अनुरोध किया। स्वामी जी ने उनसे इसमें उपस्थित न हो सकने के लिए क्षमा-याचना की; क्योंकि वह कुछ अन्य लोगों को उन्हीं दिनों में उनके समारोहों में सम्मिलित होने का पहले ही वचन दे चुके थे। श्री माँ आनन्दमयी ने मृदु मातृसुलभ खेदपूर्ण वाणी में अपनी मनोव्यथा व्यक्त की कि अन्ततः बाबा नहीं सम्मिलित होंगे। इस पर स्वामी जी ने मुखरित स्वर में बल देते हुए कहा, “यदि श्री माँ की ऐसी इच्छा होगी तो यह सेवक निश्चय ही दोनों स्थानों में उपस्थित होगा।" स्वामी जी का, जो असाधारण कार्यों का संकेत सबके समक्ष न प्रकट करने को सदा सावधान रहते हैं, ऐसा दृढ़ कथन, महान् सन्त जिस अतिभौतिक स्तर पर सम्पर्क करते हैं, न केवल उसे व्यक्त करता है अपितु वह महान् सम्मान भी प्रकट करता है जिसे वह उनके प्रति रखते हैं।
जैसा कि ऊपर बताया गया है स्वामी जी श्री आनन्दमयी संघ के साधना-कार्यक्रमों में प्रायः सम्मिलित होते हैं। एक बार संयम-सप्ताह में सम्मिलित होने के लिए वृन्दावन में माँ के आश्रम पहुँचे। जब उनके पहुँचने का समाचार पूजनीया माँ को दिया गया तो वह उनका स्वयं स्वागत करने के लिए तुरन्त बाहर आयर्थी। स्वामी जी ने जब उन्हें अपनी ओर आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तत्काल भूमि पर दण्डवत् प्रणाम किया। श्री माँ एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित-सी रह गयौं। तत्पश्चात् उन्होंने सानुकम्पा असम्मति प्रकट करते हुए कहा : "बाबा, आप क्या कर रहे हैं।" स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा; क्योंकि वहाँ कुछ कहने के लिए था ही नहीं। वह अपनी सामान्य सत्ता में नम्रता तथा सदाचार के मानवीकरण थे। तदनन्तर श्री माँ ने समारोह के कार्यक्रम की रूपरेखा देना आरम्भ कर दिया और स्वामी जी से जानना चाहा कि क्या बह उसे 'ठीक' समझते हैं। स्वामी जी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया : "जब यहाँ श्री माँ ठीक हैं तो सब-कुछ अवश्य ही ठीक होगा।" श्री माँ खिलखिला कर हँस पड़ी और तत्पश्चात् गम्भीर स्वर में बोलीं : "यदि कहीं कुछ त्रुटि है तो बाबा स्वयं सुधार लेंगे। आखिर यह आश्रम भी बाबा का ही है।" अपने वार्ता-काल में उन्होंने स्वामी जी को स्मरण दिलाया कि अगले दिन एकादशी है। स्वामी जी ने शिष्टतापूर्वक कहा कि संयम-सप्ताह में भागीदार होने से उन्होंने पहले ही व्रत में अपना नामांकन करा दिया है। माता ने गम्भीर स्वर में कहा: "बाबा तो नित्य ही संयम की अवस्था में रहते हैं।" माँ आनन्दमयी के स्तर की भगवत्साक्षात्कार प्राप्त आत्मा का यह अर्थगर्भित कथन स्वामी जी की निरन्तर तपस्या की आभ्यन्तर अवस्था का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करता है। स्वामी जी जो कुछ भी हैं, उससे अब उन्हें उपवास तथा अन्य तपों की आवश्यकता नहीं है तथापि अन्य जिज्ञासुओं के लिए उदाहरण बनने तथा भौतिक शरीर को सतत कठोर अनुशासन में रखने के लिए वह सदा उपयुक्त बाह्य अनुशासन का पालन करते हैं। भगवान् ने गीता (३-२१,२२) में कहा है : "श्रेष्ठ व्यक्ति जो-जो आचरण करता है, अन्यान्य साधारण व्यक्ति उसका ही अनुसरण करते हैं। वह जो-कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बर्तते हैं। हे अर्जुन! त्रिलोक में मेरा कुछ भी कर्तव्य कार्य नहीं है और न कोई प्राप्तव्य मेरे लिए अप्राप्त है; फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त रहता हूँ।"
स्वामी जी के वहाँ से विदा होने के दिन पूजनीया माता जी उनके साथ सत्संग में सम्मिलित हुई। स्वामी जी तथा माता जी दोनों ही भक्तों से घिरे थे। एक भक्त ने जो छायाचित्र लेना चाहता था, स्वामी जी से माता जी के पास खिसकने की प्रार्थना की। स्वामी जी तत्परता से खिसक कर श्री माँ के बहुत निकट चले गये तथा टिप्पणी की : "क्या आप सोचते है कि मैं श्री माँ से कभी दूर हूँ? मैं सदा ही उनकी सन्निधि में हूँ।" इझस पर श्री माँ का मुख प्रफुल्ल पुस्कान से दीप्त हो उठा। फोटो लेने का काम समाप्त होने पर स्वामी जी ने चित्रकार से परिहास में कहा: "कृपया छायाचित्र की एक प्रति मुझे भी भेजिएगा जिससे मैं देखूँ कि मैं श्री माँ के कितने निकट हूँ।”
उस साधना-कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में जिज्ञासु सम्मिलित हुए। उनमें अधिकतर श्री माँ के आश्रम की पाठशाला के संस्कृत के युवक छात्र थे। उन्होंने स्वामी जी के अल्पकालिक आवास-काल में उनकी अच्छी सेवा की । स्वामी जी ने इसके मान तथा आभार के प्रतीक-रूप में उन्हें मिष्टान्न तथा फल के कुछ डिब्बे भेंट किये; किन्तु किसी ने उन्हें बताया कि साधकों को जो भोजन परोसा जाता है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ खाना उन्हें मना है। यह सुन कर स्वामी जी ने अपने एक शिष्य को भेंट के साथ श्री माँ के पास जाने तथा उस भेंट के पीछे जो उद्देश्य है, उससे उन्हें अवगत कराने का कार्य सौंपा। जब शिष्य ने श्री माँ को यह सन्देश दिया तो वह एक क्षण मौन रहीं। फिर वह तत्काल मुस्करा पड़ीं और उन्होंने कहा, “ठीक है। यदि बाबा साधना में भाग लेने वाले साधकों के लिए मिष्टान्न मँगवाने में प्रसन्न हैं तो मिष्टान्न बाबा के प्रसाद का रूप ले लेता है। मैं स्वयं उन सबको मिष्टान्न बाँदूँगी। कृपया इसे बाबा को सूचित कर दीजिए।" यह छोटा-सा प्रसंग स्वामी जी के प्रति श्री माँ का असाधारण सम्मान व्यक्त करता है। नियम अनुशासन के उद्देश्य से हुआ करते हैं; किन्तु ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं जब दिव्य स्पर्श मानवीय संस्थाओं के सामान्य नियमों के अतिक्रमण का अधिकार प्रदान करता है।
श्री माँ तथा स्वामी जी के मिलन की मंजुलता का सम्यक् वर्णन करने में शब्द असमर्थ हैं। उनका पारस्परिक प्रेम तथा आदर-भाव वस्तुतः दिव्य कोटि का है। उनका मिलन सभी पार्थिव सम्पर्कों से परे है। वह वस्तुतः दिव्य सम्बन्ध है। स्वामी जी जब कभी उनके सान्निध्य में होते हैं तो वह आनन्दातिरेक में अपने-आपको खो बैठते हैं और अन्य सब-कुछ भूल जाते हैं जो उन जैसे असाधारण सन्तुलन वाले व्यक्ति में होना निश्चय ही अत्यधिक विलक्षण तथा रहस्यमय है। एक बार सन् १९७३ में स्वामी जी नयी दिल्ली में होने वाले अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन से पूर्व श्री माँ के साहचर्य में रहने के लिए तीन दिन के लिए वृन्दावन जा रहे थे। तब तक सम्मेलन के आयोजकों ने इस अवसर को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करने के लिए श्री माँ को अपना निमन्त्रण-पत्र स्वयं दे दिया था। सदा की भाँति श्री माँ ने उन्हें कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया, विषय को विधाता की इच्छा पर छोड़ दिया। अतः आयोजकों ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि वह जब श्री माँ से वृन्दावन में मिलें तो उन्हें आमन्त्रित करने की कृपा करें। स्वामी जी ने चुपचाप उनकी बातें सुनीं; किन्तु अपना कुछ मत प्रकट नहीं किया। उन्होंने वन्दावन में श्री माँ की संगति में तीन दिन व्यतीत किये. किन्त सम्मेलन के विषय मैं उनसे कोई बात नहीं हुई। स्वामी जी के वृन्दावन से वापस आने पर आयोजक उनसे मिले तथा श्री माँ के कार्यक्रम के विषय में पूछा। इस पर स्वामी जी अकस्मात् चुप हो गये और फिर धीरे से बुदबुदाये : "मैं वृन्दावन में सब-कुछ भूल जाता हूँ। मैं किसी दूसरे लोक में था।" उन्होंने और आगे कहा : "श्री माँ के सानिध्य में मैं सब-कुछ भूल जाता हूँ।"
न्यायाधीश मुधोलकर, जो गुरुदेव के परम भक्त हैं, आश्रम में अपनी पुत्री डा. अरुणा के लिए, जो श्री आनन्दमयी की एक निष्ठावान् शिष्या हैं, एक कुटीर निर्माण कराना चाहते थे। जब भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तब माँ उसके उद्घाटन-समारोह में सम्मिलित होने के लिए आयीं। एक हृदयस्पर्शी दृश्य में उन्होंने अरुणा को स्वामी जी की पुत्री का नाम दे कर उन्हें स्वामी जी को समर्पित किया तथा लोगों को बतलाया कि बाबा जी तथा उनमें कोई भेद नहीं है। जहाँ तक श्री माँ के प्रति स्वामी जी के प्रेम तथा श्रद्धा का सम्बन्ध है, वे इतने सुविदित हैं कि उनके और अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी सुनिश्चित हैं कि माता उन अतिविरल सन्तों में हैं जो सदा सहज समाधि-अवस्था में रहते हैं। उनके लिए वह सन्त नहीं हैं, वह शुद्ध भागवत सत्ता है।
श्री माँ उत्तरकाशी जाते समय कभी-कभी शिवानन्दाश्रम आती हैं। आश्रमवासी उनके एक विशिष्ट अभ्यागम को विशेष आनन्द से स्मरण करते हैं। एक बार सन् १९७६ के ग्रीष्म-काल में उन्होंने आश्रम में अकस्मात् दर्शन दिया। स्वामी जी ने एक विशेष सत्संग में उनका स्वागत किया। श्री माँ श्रद्धेय स्वामी जी के दिव्य आनन्दातिरेक से बहुत प्रभावित हुईं। वातावरण आध्यात्मिक स्पन्दनों से अधिभारित था। अब देखें! श्री माँ स्वयं भावातिरेक में आ गयीं और उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों में अविस्मरणीय रहस्यात्मक धर्मोत्साह तथा आनन्द आपूरित करते हुए अपने प्रिय कीर्तन 'हे भगवान्! हे भगवान्!' की वर्षा की।
स्वामी जी महाराज के हीरक जयन्ती-समारोह में स्वामी जी श्री श्री माँ आनन्दमयी के उस अवसर पर पधारने की सम्भावनाओं के विषय में मुश्किल से बता सके थे कि श्री माँ सभामंच पर अकस्मात् आ उपस्थित हुई। उस समय वहाँ देखने को हृदयस्पर्शी दृश्य था. वास्तव में आध्यात्मिक नयनोत्सव था। स्नेह तथा आनन्द से पूर्ण श्री माँ पुष्पों तथा फलों की डलिया लिये हुए स्वामी के पास गयाँ। स्वामी जी तत्काल उनके प्रति अपने श्रद्धा-भाव की अभिव्यक्ति के रूप में भगवती माँ की स्तुति के कुछ स्तोत्र लय के साथ गुंजारने लगे। दोनों दिव्य व्यक्तियों ने बहुसंख्यक जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं तथा सन्तों के समर्थः रोमहर्षक रूप से अपने गहन भाव तथा सम्मान का विनिमय किया। इस अवसर पर स्वामी जी ने दैवयोग से उनके समक्ष अपना यह भाव व्यक्त किया कि वह अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं और अब उन्हें अपने इस पार्थिव शरीर को और अधिक समय तक बनाये रखने में रुचि नहीं है। आहत-हृदय पूज्य माँ ने सोत्कण्ठा बलपूर्वक कहा कि उन्हें आने वाले अनेक वर्षों तक अपनी उपस्थिति से संसार को धन्यभाग बनाते रहना चाहिए। स्वामी जी की प्रार्थना पर श्री माँ ने उपस्थित जिज्ञासुओं के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा की। हम यहाँ उसका एक लघु उद्धरण देते हैं :
जिज्ञासु-गुरु के निर्देशानुसार आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने में बाधाएँ क्यों आती हैं?
श्री माँ-यदि गुरु उपस्थित हों तो बाधाएँ स्वयमेव लुप्त हो जाती हैं। बाधा तथा गुरु परस्पर विरोधी हैं।
जिज्ञासु-ऐसा क्यों है कि सभी शिष्य अपने सार्व गुरु की कृपा समान मात्रा में प्राप्त नहीं करते।
श्री माँ-अपना पात्र उलटा रख कर वे अपने को उससे वंचित कर लेते हैं।
जिज्ञासु-जीवन का लक्ष्य क्या है?
श्री माँ- उस (भगवान्) को जानना ।
जिज्ञासु-क्या भगवान् को देखा जा सकता है?
श्री माँ-हाँ ! यदि अभीप्सा प्रखर है, यदि जिज्ञासु वास्तव में गम्भीर है, तो उसका दर्शन यहाँ और अभी हो सकता है। बात तो यह है कि हम उसके लिए पूरे मन से पिपासा नहीं रखते जब कि हमारी अशेष सत्ता की माँग करते हैं।
गॉडल में हाल की उनकी भेंट के समय एक भक्त ने श्री माँ से उनके आत्म-साक्षात्कार-प्राप्ति के समय के विषय में प्रश्न किया। श्री माँ के कुछ कहने के पूर्व ही स्वामी जी ने टिप्पणी की : "यह प्रश्न तो वैसा ही है जैसे भगवान् कृष्ण से प्रश्न करना कि उन्हें भगवत्साक्षात्कार कब हुआ ?" श्री माँ का स्वामी जी के प्रति जो स्नेह तथा आदर के भाव का हृदयग्राही संयोग है, उसका अनुभव इस लेखक ने सत्ताईसर्वे अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन के लिए उन्हें आमन्त्रण हेतु कनखल में उनके दर्शन करते समय किया। श्री माँ ने अस्वस्थता के कारण उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा अपने से आग्रह न करने का अनुरोध किया। जब लेखक ने उल्लेख किया कि स्वामी जी समारोह की अध्यक्षता करेंगे तथा उनसे उनके आशीर्वाद की याचना की तो उनके व्यवहार में तत्काल सुस्पष्ट परिवर्तन आ गया। उन्होंने अपने मधुर तथा गुंजायमान स्वर में लेखक को 'चिदानन्द बाबा' को अपना 'ॐ नमो नारायणाय' कहने के लिए कहा तथा गम्भीरतापूर्वक बल दे कर कहा कि स्वामी जी की उपस्थिति मात्र से ही सम्मेलन अवश्यमेव सुखभागी होगा तथा उनकी शुभ कामनाएँ सदा ही स्वामी जी के सभी अध्यवसायों में हैं।
वर्षभर कार्यसमाकुल सूची तथा भूमण्डल के दूर देशों तक विस्तृत प्रवास के होते हुए भी स्वामी जी किसी-न-किसी सन्त के सान्निध्य में रहने के लिए कभी-कभी बलात् अपने को कार्यमुक्त कर लेने में सफल हो जाते हैं। ऐसे ही वातावरण की वह अभिलाषा रखते हैं, यही वह जगत् है जिसमें वह कदाचित् मानसिक धरातल पर सतत निवास करते हैं। वह जब कभी किसी सन्त से मिलते हैं तो तत्काल विनम्रता तथा शालीनता के साथ आगे बढ़ कर उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। उनका यह संदाचार सबके लिए प्रेरणादायी उदाहरण संस्थापित करता है। वह उत्कृष्ट कोटि के वेदान्ती हैं जो सदा अपने सच्चिदानन्दस्वरूप में स्थित रहते हैं; किन्तु वह परम सत्ता के सभी प्रकट रूपों की पूजा करते हैं तथा उनके उपासकों और सिद्धों को प्रणाम करते हैं।
उत्तर भारत के एक विलक्षण रहस्यवादी नीमकरोली बाबा, जो हनुमान्-सिद्ध थे, ऐसे ही एक सन्त थे जिनके प्रति स्वामी जी अत्यधिक पूज्य भाव रखते थे। बाबा जी महाराज कुमायूँ में नैनीताल के निकट कैंची ग्राम में अपने आश्रम में रहा करते थे। एक बार सन् १९७३ के शरत्काल में स्वामी जी सन्ध्यावसान के समय बाबा के आश्रम में पहुँचे। यथोचित आज्ञा ले कर जब वह अन्दर गये तो उन्होंने बाबा को एक साधारण-सा कम्बल लपेटे तख्त पर बैठे हुए पाया। बाबा ने स्वामी जी का स्वामत करते हुए कोई भाव व्यंजित नहीं किया। वह तख्त पर सामान्य रूप से बैठे रहे और उसी अवस्था में उन्होंने सौम्य दृष्टि डाल कर स्वामी जी तथा उनकी मण्डली का स्वागत किया और तख्त के पास बिछी हुई दरी पर उन्हें बैठने के लिए इशारा किया। स्वामी जी का प्रतीयमानतः निरुत्साह तथा रूखा स्वागत होने से उनके एक युवक आदर्शवादी साथी श्री योगेश बहुगुणा कुछ क्षुब्ध हुए; किन्तु स्वामी जी अपने सामान्य स्वरूप में ही रहे। उन्होंने तख्त के पास घुटने टेक कर बाबा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कुछ समय पश्चात् श्री हनुमान् की स्तुति में कुछ भजन तथा स्तोत्र




गाये। स्वामी जी के कीर्तन की समाप्ति पर प्रायः मौनावलम्बी तथा कठोर दृष्टिगोचर होने वाले बाबा ने अपने सभी शिष्यों को स्वामी जी के चरणों में नमस्कार करने का आदेश दिया और कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे एक उच्च कोटि के सन्त को साष्टांग नमस्कार करने का अनुपम अवसर खो देंगे। इस पर स्वामी जी ने अपने सहज रूप में अत्यन्त नम्रतापूर्वक बद्धांजलि हो कर कहा कि मैं तो गुरुदेव शिवानन्द का एक साधारण सेवक मात्र हूँ जो निश्चय ही एक प्रोन्नत सन्त थे। किन्तु उन्होंने अपनी अप्रतिम शैली में आगे कहा कि यदि एक व्यक्ति एक पुष्प को अपनी हथेली में यथेष्ट चिर काल तक कस कर पकड़े रखे तो उसकी सुरभि हथेली में महकती रहेगी। अतएव उनके दीर्घकालिक मंगलप्रद सम्पर्क के कारण यदि गुरुदेव के सद्गुणों की सुरभि कभी-कभी उनसे हो कर फैलती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यह चिदानन्द का ढंग है और इस प्रकार स्वामी जी अपनी बालसुलभ सरलता, नम्रता तथा वैभव से सन्त-जगत् में सुशोभित हैं।
तत्पश्चात् सौभाग्य से पूजनीय बाबा ने अपनी बगल में पड़ी हुई टोकरी से प्रसाद वितरण करना आरम्भ कर दिया। श्री योगेश बहुगुणा अपने साथ केवल सात या आठ सेब लाये थे तथा उन्हें वहाँ पड़ी हुई खाली टोकरी में उन्होंने रख दिया था, किन्तु बाबा कुल मिला कर अठारह फल बाँटने तक एक-एक कर सेब निकालते ही रहे। योगेश जी तो विस्मित हो गये। बाद में स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि यह हनुमान् की उपासना से प्राप्त सिद्धि के कारण हुआ।
उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत पहले सन् १९५३ से ही बाबा की सिद्धियों की जानकारी है जब टिहरी-गढ़वाल के तत्कालीन जिलाधीश श्री त्रिवेदी के वृद्ध पिता शिवानन्दाश्रम आये थे तथा स्वामी जी की उपस्थिति में गुरुदेव को अपने गुरु नैनीताल के श्री बाबा नीमकरोली जी के अनेक चमत्कारिक कार्यों को बतलाया था। बाबा अपनी हनुमान्-सिद्धि के द्वारा इच्छा मात्र से दूर स्थानों में अकस्मात् मूर्तरूप धारण कर सकते हैं। वे बाबा जी के प्रति बड़ा स्नेह तथा आदर-भाव रखते थे। श्री गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात् वह एक बार आश्रम में अकस्मात् आ उपस्थित हुए। जब स्वामी जी उनका स्वागत करने के लिए बाहर निकले तो वह परमाध्यक्ष कुटीर के बरामदे में पहुँच चुके थे। स्वामी जी ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया, उन्हें अन्दर ले गये तथा एक आसन पर बिठाया। बाबा जी ने दिव्य जीवन संघ द्वारा की जा रही प्रशस्त सेवाओं के विषय में अपना परम सन्तोष व्यक्त किया तथा स्वामी जी की प्रार्थना पर कुछ गरम गोदुग्ध पान किया। ऐसे मिलन के अवसरों पर ऐसा अनुभव होता था कि स्वामी जी तथा बाबा जी में किसी प्रकार का आन्तरिक सम्पर्क था। अल्पभाषी प्रकृति तथा बाह्य शुष्कता के होते हुए भी बाबा जी स्वामी जी की आध्यात्मिक महिमा से अवगत थे तथा अपनी दृष्टि तथा चेष्टा से अपना सम्मान तथा स्नेह प्रकट किया करते थे।
श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य तथा अन्य महान् आचार्यों की पीठों के धर्माध्यक्षों के प्रति स्वामी जी की श्रद्धा अनुकरणीय है। परन्तु वह स्वयं श्री शंकराचार्य के केवलाद्वैतवाद के अनुयायी हैं। कांचीकामकोटि पीठ के वरिष्ठ शंकराचार्य जगद्गुरु श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती के प्रति उनकी श्रद्धा विशेष अधिक है। एक बार सन् १९७३ में जब वह दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तब उन्होंने जगद्गुरु को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाही। उन दिनों जगद्गुरु समीप के ही एक ग्राम के शिवालय में निवास कर रहे थे। उस समय वह पूर्ण मौनव्रत का आचरण कर रहे थे। स्वामी जी उस शिशिरकालीन रात्रि में केवल एक वस्त्र पहने हुए अपने हाथों में फलों से भरी एक टोकरी ले कर मन्दिर के द्वार पर जा उपस्थित हुए। उन्होंने मन्दिर में प्रवेश किया तथा कुछ भी सूचना दिये बिना ही वरिष्ठ धर्माध्यक्ष को साष्टांग प्रणाम किया। धर्माध्यक्ष ने अपनी चेष्टा तथा दृष्टि से अपनी आनन्दप्रद आशिष दी; किन्तु आचार्य तथा स्वामी जी के मध्य कोई वार्तालाप नहीं हुआ। तथापि यह स्वामी जी के लिए पूर्णरूपेण सन्तोषजनक दर्शन था। जो लोग आत्मा के माध्यम से संलाप की क्षमता रखते हैं, उनके लिए मानव-प्राणी की भाषा कदाचित् ही कुछ महत्त्व रखती हो।
आधुनिक भारत के ऐसे ही एक अन्य सन्त ठाकुर श्री सीतारामदास ओंकारनाथ महाराज हैं जो महामन्त्र-कीर्तन की साधना को इस कलियुग के मानवों के मोक्ष के अमोघ साधन के रूप में दृढ़ विश्वास रखते हैं। महामिलन-मठ, ऐमहर्स्ट स्ट्रीट, कोलकाता, पुरी, ऋषिकेश आदि भारत के अन्य पवित्र स्थानों में उनके आश्रम हैं। एक बार जब बाबा ऋषिकेश के अपने आश्रम में थे, स्वामी जी उन्हें प्रणाम करने गये। तब से दोनों में अत्यन्त स्निग्ध तथा आकांक्षित सम्बन्ध का विकास हुआ है। स्वामी जी उनसे मिलने को इतने उत्सुक रहते हैं कि वह कभी-कभी उनके दर्शन के लिए उत्तरकाशी तक जाते हैं।
एक बार जब श्रद्धेय बाबा जी अपनी भक्त-मण्डली के साथ शिवानन्दाश्रम आये तो स्वामी जी विदेश गये हुए थे। उन्हें स्वामी जी की विदेश यात्रा के विषय में पता चला। उन्होंने स्वामी जी के एक शिष्य को एक लम्बी लाठी प्रदान की जिसमें शिर से पैर तक देवनागरी लिपि में एकाक्षर 'ॐ' सुन्दर ढंग से उत्कीर्णित था तथा इच्छा प्रकट की कि वह लाठी स्वामी जी महाराज के विदेश से लौटने पर उन्हें उनकी ओर से भेंट की जाय। एक मास पश्चात् जब स्वामी जी आश्रम वापस आये और वह लाठी प्राप्त की तब उन्होंने इस उपहार की पूर्वपीठिका बतलायी। एक वर्ष पूर्व बाबा जब आश्रम में आये थे तो वह अपने हाथ में एक लम्बी लाठी लिये हुए थे जिसमें शिर से पैर तक ॐ का प्रतीक था। स्वामी जी ने उसकी सुन्दर कारीगरी से प्रभावित हो कर उसकी सराहना की थी। बाबा ने तुरन्त उस लाठी को उन्हें भेंट करना चाहा; किन्तु स्वामी जी ने यह कह कर भेंट अस्वीकार कर दी कि उनके पास पहले से ही कई लाठियाँ हैं और बाबा की पदयात्रा में प्रयोग करने के लिए उनके पास केवल वही एक है। तथापि बाबा को स्वामी जी की सराहना स्मरण रही, उन्होंने उसी प्रकार की एक लाठी मँगायी और उसे अपने परवर्ती अभ्यागम के समय स्वामी जी को व्यक्तिगत रूप से भेंट करने का निश्चय किया। स्वामी जी ने उस लाठी को बाबा के प्रेम के स्मृति-चिह्न के रूप में अपनी बैठक में सुरक्षित रखा है। एक अन्य अवसर पर बाबा जी ने स्वामी जी को एक पूरा व्याघ्र-चर्म भेंट किया।
बाबा इस वैयक्तिक प्रेम के कारण ही दिल्ली में चौबीसवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन का उद्घाटन करने को सहमत हुए। उन्होंने दिव्य जीवन सम्मेलन की रजत जयन्ती में भी उपस्थित होने की कृपा की जहाँ वह दिव्य प्रेम से इतना ओत-प्रोत हो गये कि वह वहीं भाव-समाधि में प्रवेश कर गये। स्वामी जी ने, जो सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, दृढ़तापूर्वक कहा कि बाबा जी नाम-स्वरूप तथा आधुनिक भारत के भगवत्साक्षात्कार प्राप्त सन्तों में सर्वाधिक वरिष्ठ हैं।
स्वामी जी ऐसा ही महान् सम्मान कन्हनगढ़ के आनन्दाश्रम में प्रकाशमान दक्षिण भारत की एक अन्य प्रमुख आध्यात्मिक ज्योति के प्रति रखते हैं। अपने पूर्वाश्रम के प्रारम्भिक जीवन से ही आनन्दाश्रम के यशस्वी संस्थापक स्वामी रामदास के कारण उस आश्रम के लिए उनमें गम्भीर आध्यात्मिक अनुराग है। वह उस आश्रम में प्राय: जाया करते थे जिससे वह प्रिय पापा, स्वामी रामदास की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी पुण्यात्मा माता कृष्णाबाई के निकट सम्पर्क में आ गये। स्वामी जी अपने परिव्राजक-काल में सन् १९६२ के ग्रीष्मकाल में यहाँ कुछ समय तक रुके थे। इसी समय परम पूजनीया माता कृष्णाबाई को स्वामी जी का घनिष्ठ परिचय प्राप्त हुआ।
स्वामी जी स्वामी रामदास तथा माता कृष्णाबाई को एक ही समझते हैं। वह माता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुन:-पुनः आनन्दाश्रम जाते रहे हैं और प्रत्येक बार ही उनके भावपूर्ण सत्संग का लाभ प्राप्त किया है। माता जी भी स्वामी जी का बड़ा सम्मान करती हैं और उनके प्रति बड़ा ही आदर तथा वात्सल्य-भाव व्यक्त करती हैं। सन् १९७६ के अन्तिम काल में एक दिन स्वामी जी माता जी का दर्शन करने शीघ्रतापूर्वक आनन्दाश्रम पहुँचे जो नवम्बर माह से अस्वस्थ थीं। यह हृदयस्पर्शी दृश्य था। माता जी स्वयं शय्याग्रस्त होते हुए भी स्वामी जी की सुविधा की व्यवस्था की प्रत्येक अति गौण बात पर भी निरन्तर ध्यान देती रहीं। प्रबुद्ध आत्माएँ एक-दूसरे के प्रति ऐसा ही सम्मान-भाव रखा करती हैं। स्वामी जी उन्हें माँ आनन्दमयी के समान ही समझते हैं। उनके अपने शब्दों में: "माता कृष्णाबाई वात्सल्यमयी आनन्दमयी के सदृश ही हैं। मैं उनके समकक्ष किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता हूँ।"
स्वामी जी ऋषिकेश आने वाले प्रतिष्ठित सन्तों में से अधिकांश को शिवानन्दाश्रम में निमन्त्रित करते हैं। स्वामी शरणानन्द जी ऐसे ही एक सिद्ध महात्मा थे जो प्रायः प्रति वर्ष ही ग्रीष्म-काल में 'गीता-भवन' आया करते थे और एक माह तक पवित्र प्रवचन करते थे। इस अवधि में वह कभी भी किसी अन्य कार्यक्रम के लिए बाहर नहीं जाते थे; किन्तु स्वामी चिदानन्द जी के लिए अपने विशेष प्रेम के चिह्न-स्वरूप वह सदा ही एक-दो दिन के लिए शिवानन्दाश्रम आते तथा प्रवचन करते और वहाँ के साधकों को आशीर्वाद देते थे। वह दिव्य जीवन संघ के तत्कालीन सचिव स्वामी प्रेमानन्द जी महाराज के आद्यतम प्रेरकों में से एक थे। अतएव शिवानन्दाश्रम आने तथा उन्नतकारी सत्संग में चिदानन्द तथा अन्य स्वामी लोगों से मिलने में उन्हें द्विगुणित प्रसन्नता होती थी। शरणानन्द जी चिदानन्द जी से श्री माँ आनन्दमयी के संयम-सप्ताह में भी मिला करते थे। स्वामी जी ने २५ दिसम्बर १९७४ को उनकी महासमाधि को सन्त-जगत् में रिक्तता उत्पन्न होना माना।
माँ आनन्दमयी के प्रख्यात संयम-सप्ताह के अवसर पर ही स्वामी जी ने श्रीमद्भागवत के लब्धप्रतिष्ठ व्याख्याकार स्वामी अखण्डानन्द जी महाराज का दर्शन किया था। अखण्डानन्द जी स्वामी जी का विनम्रता के साक्षात् अवतार के रूप में सम्मान करते हैं। हरिद्वार में श्रोताओं में सम्भाषण करते हुए उन्होंने कहा : "स्वामी चिदानन्द साक्षात् विनम्रता की मूर्ति हैं। यदि कोई व्यक्ति विनम्रता को मनुष्य के रूप में देखना तथा विनम्र बनने का पाठ सीखना चाहता है तो उसे चिदानन्द के पास जाना चाहिए। इस युग में ऐसा असाधारण विनयशील सन्त मिलना दुर्लभ है।" स्वामी जी के सम्बन्ध में स्वामी शरणानन्द जी के भी ऐसे ही विचार थे। वास्तव में विनम्रता ही स्वामी जी के व्यक्तित्व का प्रमाण-चिह्न है। यह गुण ही सन्त-जगत् में इन्हें अमानित्व के अवतार के रूप में अन्य सन्तों से पृथक् करता है।


गुरुदेव के समकालीन सन्तों के साथ वह शिष्य-सुलभ व्यवहार करते हैं। वह उनकी आज्ञा का वैसे ही पालन करते हैं जैसे अपने गुरुदेव की आज्ञाओं का करते थे। परमार्थ निकेतन के श्री स्वामी शुकदेवानन्द जी महाराज तथा श्री स्वामी भजनानन्द जी महाराज तथा शान्ति-आश्रम के श्री स्वामी ओंकार जी महाराज जैसे महात्माओं के प्रति इनका श्रद्धास्पद व्यवहार अनुकरणीय है। स्वामी शिवानन्द तथा स्वामी ओंकार के बीच आध्यात्मिक प्रेम का निकट का सम्बन्ध तथा ईश्वराश्रित दिव्य मैत्री-भाव रहा है; अतः स्वामी चिदानन्द जी आन्ध्र प्रदेश की तोतापल्ली पहाड़ी पर स्थित ओंकार स्वामी के आश्रम में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रायः जाते रहते हैं।
एक बार स्वामी जी एकादशी के दिन शान्ति-आश्रम में अतिथि थे। ऐसा हुआ कि उस दिन स्वामी ओंकार ने इस अनुरोध के साथ ज्ञानेश्वरी माता जी के हाथ कुछ भोजन भेजा कि स्वामी जी उसमें से कुछ-न-कुछ पदार्थ ग्रहण करें। स्वामी जी, जो ऐसे दिनों में ठोस भोजन नहीं करते हैं, मुस्कराये तथा वहाँ उपस्थित अपने भक्तों को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने थाली में से प्रसाद-रूप में भोजन करना आरम्भ कर दिया। किन्तु उन्होंने अगले दिन पुनः उपवास किया। यहाँ उनके इस कार्य में प्रदर्शित सूक्ष्म विचार ध्यान देने योग्य है। वह एक वरिष्ठ महात्मा की इच्छाओं के पालन को प्रथम तो नम्रतापूर्वक मान लेते हैं और अपने नियमों को भंग करते हैं और अगले ही दिन स्वेच्छा से उन नियमों को पुनः अपने ऊपर लागू कर देते हैं।
गुरुदेव की तपोभूमि दूर तथा निकट से प्रचुर संख्या में सन्तों को आकर्षित करती रही है। वे मुख्यतः स्वामी जी के दिव्य व्यक्तित्व से आकर्षित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि गुरुदेव की महासमाधि से उत्पन्न रिक्तता की उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी ने योग्य रीति से पूर्ति कर दी है। मोक्ष-आश्रम, नैमिषारण्य के जगदाचार्य स्वामी नारदानन्द गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात् प्रायः आश्रम में आते हैं। वह कहा करते हैं कि स्वामी चिदानन्द 'गंगा की धारा' हैं। कभी-कभी वह उनका उल्लेख 'प्रेम की गंगा' के रूप में करते हैं। गंगा माता की भाँति ही वह शीतल तथा मधुर, गम्भीर तथा शान्त रूप से गतिमान तथा इस पुण्य भूमि के सुविस्तृत क्षेत्रों को सम्पोषित करते हैं। नारदानन्द जी कहते हैं : "आपने शिवानन्द को खो दिया है, किन्तु आपने चिदानन्द में शिवानन्द को प्राप्त कर लिया है। उदारता तथा निस्स्वार्थता में चिदानन्द शिवानन्द के समान हैं। चिदानन्द जी ने कभी वेदान्त की शिक्षा नहीं ली, किन्तु उनके प्रवचन वैदिक ज्ञान से ओत-प्रोत होते हैं। वह वेदस्वरूप हैं।"
स्वामी जी सन्त के दर्शन करने का कोई भी अवसर, यदि उपलब्ध हो तो हाथ से जाने नहीं देते। लोक-प्रतिष्ठा, संस्था का विस्तार, सम्प्रदाय का नाम अथवा शिष्यों की संख्या-ये सब उनके लिए महत्त्व के विषय नहीं हैं। एक सन्त चाहे मठवासी हो अथवा अरण्यवासी, सार्वजनिक जीवन-यापन करता हो अथवा संन्यास का-उनके लिए समान रूप से प्रलोभक है। इस भाँति उन्होंने पवनार में आचार्य विनोबा भावे का दर्शन किया तथा उनको उसी प्रकार प्रणाम किया जैसा कि किसी वरिष्ठ संन्यासी को करते हैं।
उड़ीसा की अपनी अनेक यात्राओं की अवधि में स्वामी जी एक रहस्यवादी सन्त नामाचार्य श्री श्री बया बाबा के विषय में सुनते रहते थे जो बारह वर्ष से अधिक समय तक मौनी साधक रहे थे। बया बाबा जी श्री रामदास महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी तथा भुवनेश्वर के कल्पतरु-आश्रम के संस्थापक हैं। बाबा जी तथा स्वामी जी का मिलन रोचक परिस्थितियों में हुआ। रामदास बाबा जी की जन्म-शताब्दी द्रुतगति से समीप आ रही थी; अतः बया बाबा के शिष्य इस अवसर पर आश्रम में किसी वास्तविक विशिष्ट आध्यात्मिक व्यक्ति के अभ्यागम का प्रबन्ध करने को उत्सुक थे। बया बाबा की भी ऐसी ही स्निग्ध तथा सुभग इच्छा थी। ऐसा लगता है कि दैवकृत व्यवस्था से, जो पहले ही की जा चुकी थी, वह अवगत थे। महाबलीपुरम् से भुवनेश्वर वापस आने पर स्वामी जी अकस्मात् हवाई पत्तन से सीधे कल्पतरु-आश्रम में अन्तर्मुखी सन्त के दर्शन करने के लिए चल पड़े। दोनों सन्तों ने एक-दूसरे के सम्मुख सही अर्थों में भूमि पर लेट कर दण्डवत् प्रणाम किया तथा दीर्घकाल तक मौन वार्तालाप करते हुए एक साथ रहे। अन्त में बाबा जी ने स्वामी जी से अपने गुरुदेव श्री रामदास महाराज के जन्म-शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने के लिए आश्रम की शोभा बढ़ाने का हार्दिक तथा विनम्र अनुरोध किया। स्वामी जी ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी और उद्घाटन समारोह के लिए वहाँ पुनः आये। कार्यक्रम की समाप्ति पर स्वामी जी हस्बमामूल बाबा के पास गये और अपनी स्वाभाविक शिष्ट विधि से बाबा की कृपा की याचना की। इस पर वयोवृद्ध बाबा जी, जो उस समय प्रायः शय्याग्रस्त थे, शारीरिक आयास के बावजूद भी मानपुरःसर कृतज्ञता से उठ खड़े हुए तथा स्वामी जी के चरणों में यथार्थ अर्थों में नतमस्तक हो गये। यही स्वामी जी की प्रार्थना का बाबा जी का उत्तर था।
इस प्रकार चिदानन्द सन्त-समूह में चमकते हैं। सन्तजन उन्हें अपना अमित प्रेम तथा आदर प्रदान करते हैं। सन्तों की मान्यता निश्चय ही धार्मिक व्यक्ति की उपलब्धि का परम महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है; किन्तु चिदानन्द ऐसी मान्यता की न तो आकांक्षा रखते हैं और न अपेक्षा ही। तथापि सन्त-जगत् में उनका विशिष्ट स्थान असंख्य साधकों के लिए बहुत ही अर्थपूर्ण तथा शिक्षाप्रद है। वह परिव्राजकों तथा मठवासियों के लिए एक आदर्श संन्यासी, व्यावहारिक लोकोपकारकों के लिए पददलितों के मित्र, साक्षात्कार-प्राप्त ज्ञानियों के लिए एक व्युत्पन्न तथा व्यावहारिक वेदान्ती और अगण्य भक्तों के लिए पराभक्त हैं।
अष्टम अध्याय
पददलितों के मित्र
"ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।
--सब प्राणियों के हित में निरत व्यक्ति मुझ (ईश्वर) को प्राप्त कर लेते हैं" (गीता : १२-४)।
चिदानन्द सेवा के लिए ही जीते हैं। उन्होंने इस पार्थिव जगत् में अपना सम्पूर्ण जीवन प्रभु के सृष्ट जीवों की निरन्तर सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। वह पतितों के उदात्त उद्धारक तथा पीड़ितों की चिन्ता करने वाले उनके मित्र हैं। इस जन्मजात सन्त के दिव्य हृदय से सभी जीवधारियों के लिए अक्षय परिमाण में करुणा निस्सृत होती है। ऋषिकेश तथा उसके परिसर के अभागे कुष्ठियों के लिए तो यह साक्षात् परित्राता ही रहे हैं। अपने सम्बन्धियों द्वारा भी निन्दित, अभिशप्त तथा बहिष्कृत इन सजातीय व्यक्तियों के प्रति उनकी दयालुता तथा सहानुभूति सम्पूर्ण मानव जाति के लिए सेवा तथा परोपकार का एक प्रेरणादायी पाठ रहेगा। आध्यात्मिक आचार्य तथा सन्त तो अनेक हुए हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत हानि उठा कर भी जिज्ञासुओं के मार्ग को प्रकाशित किया है; किन्तु उनमें अल्पसंख्यक व्यक्ति ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने चिदानन्द के समान पूर्ण समर्पण-भाव से विकलांगों तथा रोगग्रस्तों के सहानुभूतिपूर्ण शारीरिक देखरेख के कार्य में आजीवन अपने को लगाये रखा हो। महापुरुषों में यीशु, बुद्ध, गान्धी, डैमियन, चिदानन्द बहुत ही कम संख्या में हैं जो इन सभी वैविध्य के मध्य परमैक्य का साक्षात्कार कर सामाजिक तथा मानवीय अभिरुचियों की मर्यादाओं से ऊपर उठते हैं तथा इस संसार के घोर पापी, निकृष्टतम कुत्सित तथा पीड़ित प्राणियों को गले लगाते हैं। चिदानन्द ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल से ही इन हतभाग्य प्राणियों के लिए जो असाधारण सहानुभूति तथा चिन्ता प्रदर्शित की, उस पर इससे पूर्ववर्ती एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। एक कुष्ठी की कुछ अस्थायी सहायता तथा देखभाल से सन्तुष्ट न रह कर उन्होंने उसके लिए अपने घर के अहाते में एक झोपड़ी बनवायी तथा उसका योग-क्षेम वहन किया। ऐसा करना उनके लिए स्वाभाविक ही था और ऐसा उन्होंने उस समय किया जब वह अल्पवयस्क ही थे। सार्वलौकिक साहचर्य, आत्मिक एकता तथा सार्वभौम प्रेम की दृढ़ धारणा ने उन्हें न केवल मानवों में अपितु पक्षियों, पशुओं तथा चतुर्दिक् अलक्षित रूप से चलने तथा रेंगने वाले कीटों में भी रोगियों तथा दीनों की सेवा करने को प्रेरित किया। अतएव एकान्त, मौन तथा साधना के लिए अपने घर तथा परिजनों को त्याग कर गंगा के तट पर आ जाने पर भी अपने नये घर के चतुर्दिक् के वातावरण को विदीर्ण करने वाले घोर व्यथा के क्रन्दन को अनसुनी न कर पाना उनके विषय में स्वाभाविक ही था। उन्होंने इसे चित्त-विक्षेप के रूप में देखने अथवा इसके प्रति वेदान्तिक उदासीनता का भाव उत्पन्न करने के बजाय सक्रिय साधना तथा पूजा के रूप में, सार्वभौमिक प्रेम की सामान्य अभिव्यक्ति के रूप में संवेदनाशील सेवा को अपनाया। प्रतिकूल प्रकृति तथा उदासीन मानवों से समान रूप से परित्यक्त बहुत बड़ी संख्या में कुष्ठियों को वहाँ किसी प्रकार अपने दुःखद जीवन को घसीटते देख कर वह अत्यधिक द्रवित हो उठे। उनकी दुर्दशा निश्चय ही अवर्णनीय थी। उन्हें रास्ते के किनारे पर तीर्थयात्रियों से जो कुछ भिक्षा-रूप में मिल जाता, उसी से वह किसी-न-किसी तरह अपने शरीर तथा प्राण को बचाये रखते थे। कुष्ठरोग के साथ-साथ उनमें अनेक प्रकार की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक वेदनाएँ प्रवेश कर गयी थीं। उनमें से अनेक विविध प्रकार के अन्य रोगों से पीड़ित थे। उदाहरणार्थ उनमें से अधिकांश के उदर-रोग थे। वे प्रायः निमोनिया तथा क्षय रोग से आक्रान्त होते थे। असहनीय ठिठुराने वाली शीत ऋतु में वह पर्वतीय नदी चन्द्रभागा के तट पर जीर्ण-शीर्ण घिनावनी झोपड़ियों में सोने के लिए चले जाते थे। उनमें से अधिकतर तो जब तक सम्भव होता, सड़क के किनारे पड़े रहना अधिक पसन्द करते थे।
अपने अभ्यासगत सायंकालीन भ्रमण के समय स्वामी जी ने सड़क के किनारे भिक्षा माँगते हुए कुष्ठरोगियों की पंक्तियाँ देखीं। उनके भाग्य को सुधारना शीघ्र ही उनकी चिन्ता का मुख्य विषय बन गया। यद्यपि कुष्ठी गैरिक वस्त्रधारी संन्यासी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते थे; किन्तु यह युवा संन्यासी उनका परम मित्र तथा परित्राता बन गया।
सन् १९४३ के प्रारम्भिक दिनों में जब स्वामी जी शिवानन्द धर्मार्थ औषधालय के कार्यभारी थे तब उन्हें कुष्ठियों की कुछ सार्थक सेवा प्रदान करने का अवसर स्वतः प्राप्त हो गया। उन दिनों बेचारे कुष्ठियों के लिए औषधालय भी वर्जित क्षेत्र हुआ करते थे। इन बेचारों को एकमात्र चिकित्सीय सेवा जो उपलब्ध थी वह था थोड़ा-सा टिंचर आयोडिन जिसे एक राजकीय औषधालय में आयुर्वेदिक औषधि वितरण करने वाले वैद्य उन्हें देते थे। बस इतना ही सब-कुछ था। कोमल हृदय स्वामी जी के लिए यह सब बहुत ही दुःखद विषय था और उन्होंने उनके स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना आरम्भ
पददलितों के मित्र कर दिया। वह स्वयं ही उनकी झोपड़ियों तक उनके लिए औषधियाँ ले जाते थे। जब कुष्ठियों को पता चल गया कि उन्हें प्रेम, उपशम तथा आशा लाने वाला मनुष्यों में एक देवदूत है, उनके शरीर, मन तथा आत्मा का उपचार करने वाला डाक्टर है तथा औषधालय के कार्यभारी स्नेहशील ब्रह्मचारी से औषधियाँ तथा परामर्श उपलब्ध हो सकते हैं तो वे बड़ी संख्या में औषधालय में आने लग गये। इस प्रकार शिवानन्द धर्मार्थ औषधालय कुष्ठियों के लिए एक कार्यसमाकुल चिकित्सालय बन गया। नरेन्द्रनगर के उदार महाराजा कुष्ठरोगियों के लिए प्रथमोपचार का सामान तथा मरहमपट्टी की सामग्री उपलब्ध कराते थे। उस समय कुष्ठियों को एकमात्र यही व्यवस्थित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध थी। अब स्वामी जी अपना रोगहर हाथ ले कर साक्षात् भगवान् के रूप में उनके समक्ष आये और स्वामी जी के लिए इन पीड़ितों के रूप में स्वयं भगवान् उपस्थित हुए। अतएव वह लोकोपकारी कर्म वास्तव में सर्वशक्तिमान् प्रभु की सेवा थी। स्वामी जी जब कुष्ठरोग की विकसित अवस्था में रोगियों के खुले व्रणों की मरहमपट्टी करने में संलग्न रहते तो उनके नेत्रों से करुणा व्यक्त होती तथा उनके मुख से गम्भीर वात्सल्य-प्रेम चतुर्दिक् प्रसरित होता था। स्वामी जी उनके लिए प्रातः बड़े सबेरे ही औषधालय में उपलब्ध रहते जिससे भिक्षा-संग्रह करने के लिए वे खाली हो जायें और औषधालय में आने वाले अन्य रोगियों के मन में उनकी उपस्थिति से विक्षोभ न हो। औषधालय में कुष्ठियों की इनकी महती सेवा से चिकित्सा-शास्त्र के विशेषज्ञों में भी विस्मय तथा श्लाघा का भाव उत्पन्न होता। स्वामी जी रोगियों को जिस प्रकार रोग-मुक्त करते थे, उसे देख कर भारतीय सेना की चिकित्सा-सेवाओं के तत्कालीन निर्देशक मेजर जनरल ए. एन. शर्मा चकित रह गये। उन्होंने कहा कि यह युवक ब्रह्मचारी सामान्य व्यक्ति नहीं है।


एक पंजाबी सन्त कुष्ठरोग से पीड़ित थे। रोग गम्भीर रूप से बढ़ चला था। वह कुछ दिनों तक तो सड़क पर ही दिन काटता रहा। अन्त में उसने एक दिन स्थानीय पाठशाला के एक अध्यापक से उन्हें शिवानन्दाश्रम पहुँचाने की प्रार्थना की। उस अध्यापक की सहायता से वह रोगी आश्रम के द्वार तक पहुँच पाया। उस समय रात्रि के दश बज चुके थे। जब स्वामी जी को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक रोगी उनकी प्रतीक्षा कर रहा है तो रात्रिकालीन सत्संग समाप्तप्राय था। स्वामी जी हाथ में चोरबत्ती लिये हुए बाहर आ गये और उस स्थान पर गये जहाँ रोगी लेटा हुआ था तथा उसकी दयनीय दशा देखी। वह उसे तत्काल योग-साधना-कुटीर के बरामदे में ले गये और गुरुदेव को सन्देश दे कर उस रोगी को आश्रम के अन्दर स्थान देने के लिए उनकी अनुमति माँगी। गुरुदेव स्वयं दया-भाव से अभिभूत थे। उन्होंने आवश्यक अनुमति दे दी।
उसके पश्चात् स्वामी जी ने उस रोगी की सेवा-सुश्रूषा इतने प्रेम तथा परवाह के साथ आरम्भ कर दी कि उससे बढ़ कर माँ भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने उस रोगी के लिए, जिसने उनके चरणों का आश्रय लिया था, अपने कुटीर के सामने ही एक झोपड़ी बनवा दी। उन्होंने पन्दरह दिन तक कार्य किया तथा क्लोरोफार्म, तारपीन तथा अन्य औषधियाँ लगा कर रोगी के शरीर से रोगाणुओं को दूर करने में वह सफल हुए। वह अपने हाथों से उसके व्रणों की मरहमपट्टी करते थे। उन्हें प्रसन्नता थी कि उन्हें इस महान् सेवा में पुत्तूर के श्री सूर्यनारायण का सहयोग प्राप्त था। मित्र, चिकित्सक, परिचारिका, रसोइया तथा भंगी की संयुक्त भूमिका निभाते हुए वह लगातार कई महीनों तक यह सेवा करते रहे। उस अभागे प्राणी का मल-मूत्र भी वह साफ करते थे। जब नाई ने उसके बाल काटने से इनकार कर दिया तब उन्होंने स्वयं ही यह कार्य किया। नियत तालिका के अनुसार उन्हें उस रोगी को दिन में आठ या दश बार खिलाना पड़ता था। आखिरकार, वह रोगी निस्सहाय के रूप में नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई न था, अतएव उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होता उसे यह विनम्र भक्त बड़ी ही परवाह, प्रेम तथा श्रद्धा के साथ करता था।
एक दिन सन्ध्या के अवसन्नप्राय होने पर आँधी आयी जिससे रोगी की झोपड़ी नष्ट हो गयी। कुछ-न-कुछ अस्थायी प्रबन्ध करना था; किन्तु वहाँ कौन था जो उस असहाय प्राणी की ऐसे विषम समय में देख-भाल करता! उसके एकमात्र मित्र, सहानुभूतिशील स्वामी जी उस रोगी को एक समीपवर्ती गुफा में ले जाने के लिए आँधी रहते ही अपने कुटीर से बाहर आ गये। वह रोगी की खाट तथा अन्य सामान भी अपने कन्धों पर ले गये। आगामी दिवस को उन्होंने उस छोटी-सी गुफा को साफ-सुथरा किया और तब उस व्यक्ति के लिए एक नयी झोपड़ी बनवायी। तत्पश्चात् पुनः वही मूक सेवा धारा की भाँति अपने सामान्य तथा सहज प्रवाह के साथ चलती रही। वहाँ न तो कोलाहल था और न आत्माभिनन्दन अथवा थकान की भावना ही। यह सब सार्वभौमिक प्रेम की भावना से परम प्रशान्ति से किया गया। रोगी कभी-कभी मिष्टान्न खाने की इच्छा व्यक्त करता । स्वामी जी उसके निर्देशानुसार उन मिष्टान्नों को तैयार करते और उसे स्फूर्तिदायक स्नान कराने के पश्चात् स्वयं उसे स्नेह पूर्वक परोसते। दूसरों के उपहास की उपेक्षा करते हुए तथा सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार करते हुए, अन्त में वह उस रोगी को रोगमुक्त करने में सफल हुए।
गुरुदेव ने टिप्पणी की कि स्वामी जी ने तो एक चमत्कार कर दिखाया। रोगी साधु, जिसके बचने की आशा अन्य लोगों ने छोड़ दी थी, अब स्वयं इधर-उधर चलने तथा स्नान करने में सक्षम हो गया। गुरुदेव ने बड़े ही प्रशंसात्मक भाव से कहा, "चिदानन्द जी ने अपनी प्रेममयी सेवा से उसे नवजीवन प्रदान किया है।" उन्होंने और आगे कहा कि वह स्वयं भी ऐसी पूर्ण भक्ति के साथ उसकी सेवा न कर पाये होते। एक बार जब स्वामी जी इस निस्सहाय-रूप भगवान् की पूजा में तल्लीन थे तब गुरुदेव ने अपने एक वरिष्ठ भक्त पन्नालाल जी को ध्यान दिलाया कि वह स्वयं देखें कि स्वामी जी किस प्रकार कर्म को पूजा में रूपान्तरित कर रहे हैं। जब स्वामी जी सितम्बर १९५० में अखिल भारत यात्रा में गुरुदेव के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे तब उस रोगी ने स्वयं ही सूचित किया कि वह किसी मार्गरक्षी की सहायता से अमृतसर में अपने मठ में जाना अधिक पसन्द करता है। स्वामी जी ने उसे उसके मार्ग-व्यय के लिए रुपये दिये और इस प्रकार परम सन्तोष के साथ अपनी सेवा पूर्ण की। रोग-मुक्त करने का उनका यह चमत्कारिक कार्य शिवानन्दाश्रम की सेवाओं की गाथा में बहु-उद्धृत उदाहरण बन गया है। स्वयं गुरुदेव ने अखिल भारत यात्रा में अपने व्याख्यानों में स्वामी जी की इस असाधारण सेवा का कई बार उल्लेख किया था।
अखिल भारत यात्रा से वापस आने के पश्चात् स्वामी जी ने कुष्ठरोगियों की सेवा के कार्य को तीव्र कर दिया। उनके दीर्घकालिक प्रयास के परिणामस्वरूप कुछ भूमि प्राप्त की जा सकी तथा ब्रह्मपुरी की कुष्ठ-बस्ती का निर्माण हो सका ।
सन् १९५२ में एक दिन मूसलाधार वर्षा हुई और चन्द्रभागा ने अपने किनारों को तोड़ डाला। मुनिकीरेती के निकट की कुष्ठ-बस्ती की कई झोपड़ियाँ बह गयीं। दूसरे दिन प्रात:काल ही सभी कुष्ठी शिवानन्दाश्रम के द्वार पर आ गये। चिदानन्द जी एक बार पुनः उनके पराक्रमी रक्षक बने। वह गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी के पास उनके परामर्श के लिए गये। उन्होंने अनुभव किया कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम उन सबके लिए ताजा गरम भोजन का प्रबन्ध किया गया। तत्पश्चात् वह बाहर गये तथा जिला अधिकारियों से उन्होंने सम्पर्क किया। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा का भी आयोजन किया और कुष्ठियों की विकट समस्या की ओर सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। सभा में यह निर्णय किया गया कि एक कुष्ठ-निवारक-समिति स्थापित की जाय। जिलाधीश इस समिति के पदेन अध्यक्ष थे; नगरपालिका का अध्यक्ष, स्वास्थ्य-अधिकारी, स्वामी जी, गीता-भवन के प्रधान, कालीकमली वाला क्षेत्र के मन्त्री तथा कुछ अन्य लोग निर्वाचित सदस्य थे। इस भाँति स्वामी जी के व्यक्तित्व के प्रेरक-बल ने ही सामान्य जनता तथा स्थानीय जिला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। उनके प्रयत्नों से टिहरी गढ़वाल जिले की प्रथम कुष्ठ-निवारक-समिति संघटित हुई।
कुष्ठियों को खाद्यान्न वितरण करने के लिए धन-संग्रह किया गया। यह प्रतिबन्ध रखा गया कि कुष्टी अपनी जीविका के साधन के लिए सड़क के किनारे नहीं बैठा करेंगे। समिति ने उन्हें हिमालय में पाँच मील की दूरी पर ब्रह्मपुरी नामक स्थान में भेजने का निर्णय किया। यह स्थान उनके लिए ही निर्वृक्ष किया गया था। नयी कुष्ठ-बस्ती के लिए अनेक समस्याएँ थीं। वर्तमान निवास स्थानों की सफाई करानी थी, चिकित्सा की सुविधाएँ सुनिश्चित करनी थीं तथा स्वावलम्बी बनाने वाली पुनर्वास की परियोजनाएँ आरम्भ करनी थीं। राजकीय स्तर पर किये गये स्वामी जी के प्रयत्नों को प्रथम बार सफलता प्राप्त हुई। जिला अधिकारियों ने बस्ती के लिए एक प्रशिक्षित कुष्ठनिवारक चिकित्सक-सह-कार्यकर्ता की सेवाएँ उपलब्ध कीं। इससे रोगियों के आनन्द तथा कृतज्ञता की सीमा न रही। ऐसी घटना उनके साथ पहले कभी नहीं घटी थी। उनकी देख-भाल के लिए एक व्यक्ति का नियुक्त किया जाना उनके लिए एक असाधारण घटना थी। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने विस्मय तथा कृतज्ञता से उद्घोषित किया : "यह स्वर्गदूत है जो हमारे लिए नीचे उतर आया है।" आने वाला व्यक्ति निश्चय ही एक अभिजात तथा समर्पित निस्स्वार्थ कार्यकर्ता थे। उनका नाम रवीन्द्रकुमार मित्तल था तथा उन्हें गान्धी स्मारक कुष्ठनिवारक निधि, वर्धा ने प्रतिनियुक्त किया था।
स्वामी जी ने लोगों को इस समस्या को अपनी समस्या के रूप में देखने के लिए समझाने के लिए संघर्ष किया और वह इसमें सफल रहे। अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इस प्रकार का कार्य सहज ही दुष्कर हो सकता था। इसके अतिरिक्त स्वामी जी के विषय में यह भी पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि वह अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए जीवन का सब-कुछ त्याग कर आश्रम में आये थे। इस सामान्य समयसारिणी के विस्थापन की सहज ही कल्पना की जा सकती है; किन्तु जिस कार्य से अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता अथवा आध्यात्मिक जिज्ञासु व्यथित तथा पराभूत हुए होते उससे वह सदा की भाँति ही अखिन्न, प्रशान्त तथा निर्भीक बने रहे। उन्होंने इन सबको भगवान् की पूजा के रूप में माना और जो उस महान् आध्यात्मिक ऊँचाई पर प्रतिष्ठित हो चुका हो उसके लिए कोई भी प्रवृत्ति वास्तव में चित्त-विक्षेप का कारण नहीं बन सकती। ब्रह्मपुरी में नयी कुष्ठ-बस्ती आरम्भ करने के लिए स्वामी जी के नेतृत्व में आवश्यक कार्यवाही की गयी तथा सन् १९५९ में कुष्ठी अपनी नवीन निवासीय झोपड़ियों में स्थानान्तरित कर दिये गये।
इन अभागी आत्माओं के प्रति स्वामी जी की सेवा से प्रचुर संख्या में विदेशी भक्तों में गहरा प्रशंसा-भाव उत्पन्न हुआ। यह प्रभाव गुरुदेव के निर्देशानुसार नयी दुनिया में उनके अभ्यागम के पश्चात् और भी तीव्र हो गया। निस्स्वार्थ सेवा पर उनके प्रवचन का माता सीता फ्रेंकेल, माता सिमोनेटा तथा अन्य भाग्यशाली आत्माओं पर सशक्त प्रभाव पड़ा। माता सीता प्रथम व्यक्ति थीं जो इस निस्स्वार्थ सेवा के महान् यज्ञ में उदारता तथा प्रचुरता से दान देने के लिए आगे आयीं। माता सिमोनेटा एक अन्ताराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त महिला थीं जो प्रमुख भूषाचार अभिकल्पक के रूप में प्रचुर धन अर्जन करती थीं। वह पैरिस में स्वामी जी का भाषण सुन कर निस्सहायों की सेवा करने के लिए अपना शेष जीवन अर्पित करने को अकस्मात् प्रेरित हुईं। स्वामी जी के प्रवचन से उन पर विद्युत् गति से प्रभाव पड़ा। उन्होंने बताया कि यह छाती में धक्का लगने जैसा था। उनके अपने ही शब्दों में: "ऐसा कम्पन-इससे पूर्व मैं इस प्रकार के किसी भी कम्पन से कभी भी परिचित न थी। उस क्षण से मैं उनकी हो गयी।"
जब स्वामी जी अपनी प्रवचन- यात्रा में कैलीफोर्निया में थे उन्हीं दिनों वह (माता सिमोनेटा) अपने कारोबार के सम्बन्ध में न्यूयार्क के प्रवास पर थीं। स्वामी जी के कार्यक्रम का पता चलने पर उन्होंने अपने पत्रकार-भेंटवार्ताओं तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया तथा स्वामी जी से मिलने के लिए विमान द्वारा सैनफ्रांसिस्को जा पहुँची। स्वामी जी के साथ उनकी इस भेंट से उनमें अपूर्व परिवर्तन आया। उन्होंने अपना पुराना व्यवसाय छोड़ दिया तथा वह ब्रह्मपुरी में कुष्ठियों की तथा शरणार्थियों, निस्सहायों तथा अनाथों की सेवा में अपना जीवन अर्पित करने के लिए शिवानन्दाश्रम आ गयीं। तब से वह उनके लिए हार्दिक समर्पण तथा सहानुभूति से कार्य कर रही हैं। वह कहती हैं: "स्वामी जी में अपनी निष्ठा के कारण ही मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तथ्यों को स्वीकार करने तथा लोगों के साथ अपने सम्बन्ध के विषय में स्वामी जी ने मेरी अत्यधिक सहायता की है। मैं यह कार्य अपनी साधना के रूप में करती हूँ।"
शिवानन्दाश्रम के अपने आवास के प्रारम्भिक काल से ही न केवल आश्रम के औषधालय में आने वाले रोगियों की देखभाल करने का स्वामी जी का स्वभाव था अपितु वह सहायता की आवश्यकता रखने वाले रोगी व्यक्तियों की खोज में देहात में भ्रमण करते थे और उनकी सेवा-सुश्रूषा करते थे। उन दिनों न तो अच्छे संचार-साधन थे और न आस-पास के क्षेत्र में कोई औषधालय था। उपचार के अभाव में लोग मर जाया करते थे। उनके लिए स्वामी जी साक्षात् त्राणकर्ता थे। वह प्रायः प्रत्येक घर में पहुँच जाते और जिनको आवश्यकता होती उन सबको प्रेमपूर्वक औषधि देते थे। वह गाँव के लोगों द्वारा निष्कासित कुष्ठियों के लिए झोपड़ियाँ बनवाने की व्यवस्था करते थे। रोगियों के पास जीवन-निर्वाह का कोई साधन न था और न आवास-स्थान था। स्वामी जी उनके पास रह कर उनको भोजन कराते, औषधि देते तथा अपने हाथों से उनके व्रणों की मरहमपट्टी करते थे। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने शीघ्र ही उस इलाके में एक उदात्त आत्मा के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली और तबसे वह निर्धन तथा बीमार व्यक्तियों के कष्ट कम करने में टिहरी गढ़वाल के दूर के कोनों में भी कोई कार्य सरलता से सम्पन्न करा सकते थे।
कुछ वर्ष पश्चात् जब माता सिमोनेटा ने स्वयं को सेवा तथा साधना के लिए समर्पित कर दिया तो स्वामी जी ने ब्रह्मपुरी की बस्ती को प्रायः पूर्णतया उनके ही प्रेममय हाथों में छोड़ दिया। इस सेवानिष्ठ महिला ने बुनाई की मशीनें लगवायीं और स्वस्थ हो चुके रोगियों को उत्पादनकारी कार्य में लगाया। अब भी स्वामी जी अपने कुष्ठी मित्रों से मिलने, उन्हें आदर्श जीवन-यापन की शिक्षा देने तथा प्रसाद से उनका मुख मीठा करने के लिए कभी-कभी वहाँ जाते हैं। जब स्वामी जी ने देखा कि ब्रह्मपुरी के लिए स्थानीय सहायता अपर्याप्त है तो उन्होंने सन् १९६८ में 'डिवाइन लाइफ' पत्रिका के पृष्ठों में स्वैच्छिक योगदान के लिए एक निवेदन प्रकाशित किया। भक्तों तथा मानव-प्रेमियों ने इस माँग पर अनुकूल प्रतिक्रिया की तथा नयी धनराशि से सहायता-कार्य में गति आयी। स्वामी जी की प्रेरणा से पीड़ितों को सहायता तथा सुख पहुँचाने में दिव्य जीवन संघ ने जिला कुष्ठ-निवारक समिति को अपना सहयोग प्रदान किया।
इन्हीं दिनों सन् १९६३ में श्री रूथ याब वली तथा श्री रिचार्डसन ने लन्दन के 'सन्डे टाइम्स' में कुष्ठ-निवारण की समस्या का चित्रण किया। सन् १९७३ में श्री आर. प्रावर झाबवाला ने भी 'एशिया मैगज़ीन' तथा 'इम्प्रिण्ट' में इस समस्या तथा स्वामी जी तथा अन्य समर्पित व्यक्तियों की सेवाओं से दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में लिखा। इन पत्रकारों के प्रचार का वांछित प्रभाव पड़ा। इंग्लिश कुष्ठ-निवारक-संस्था के निर्देशक श्री फ्रांसिस हैरिस १९७३ के अक्तूबर में ऋषिकेश आये तथा उन्होंने संस्था द्वारा संगृहीत धन-राशि के उपयोग की सर्वोत्तम विधि के सम्बन्ध में स्वामी जी से विचार-विमर्श किया। उनका यह विचार था कि इंग्लिश कुष्ठ-निवारक-संस्था द्वारा संगृहीत कोष का धन किसी संस्था को ही दान में दिया जा सकता है। माता सिमोनेटा ने सुझाव दिया कि संस्था का नाम 'चिदानन्द अन्ताराष्ट्रिय कुष्ठ-निवारक-निधि' रखा जाय। इस भाँति हमारे समय के परम सहानुभूतिशील सन्त के नाम पर इस लोकोपकारी संस्था का जन्म हुआ। दिव्य जीवन संघ की सभी कुष्ठ-निवारक प्रवृत्तियाँ इस निधि के माध्यम से चलती हैं।
आश्रम के सभी विशेष दिनों में, विशेषकर शिवानन्द जयन्ती तथा चिदानन्द-जयन्ती के दिन स्वामी जी स्वयंसेवकों की एक टोली के साथ कार द्वारा ब्रह्मपुरी अथवा ढालवाला तथा लक्ष्मणझूला में विकसित कुष्ठ-बस्तियों में से किसी एक बस्ती में जाते हैं। वहाँ वह मिष्टान्न तथा फल वितरित करते तथा दक्षिणा के रूप में कुछ नकद भेंट भी देते हैं। कभी-कभी वह इन विभिन्न बस्तियों में उनके लिए खाद्यान्न तथा वस्त्रादि ले जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत चिन्ता तथा अवधान के कारण ही ढालवाला बस्ती में शनैः-शनैः जीवन की मौलिक आवश्यकताओं का सम्भरण होने लगा है। सन् १९७३ के अन्तिम भाग में सिमोनेटा, पियरे रेनियर्स, हैन्स तथा सीता फ्रेन्केल ने इन अभागे लोगों के कष्ट को कम करने में महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान की। बाद में ब्रुसेल्स, बेल्जियम के श्रीमती तथा श्रीयुत ब्रेल इस निष्काम सेवा की वेदी पर कुछ योगदान देने के लिए आगे आये। सिमोनेटा ने वहाँ कताई-बुनाई की एक औद्योगिक इकाई खोली जो दरियाँ, ऊनी स्वेटर, गुलूबन्द (मफलर) तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ तैयार करती है। उन्होंने उसके पश्चात् वहाँ चिदानन्द-कुष्ठ-उपचार-चिकित्सालय खोला। मैसर्स तिरुवल्लुवर हैण्डलूम तथा राजपलायम् के श्रीराम प्रोडक्ट्स के योगदान, मुम्बई के डा. एन. बी. सूचक तथा आदिपुर के डा. एस. जे. रुचानी द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शनों के निःशुल्क प्रबन्ध तथा मुम्बई के श्री मगनलाल पुरुषोत्तम की सहायता की इन बस्तियों के स्वस्थ विकास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
इसके अतिरिक्त स्वामी जी द्वारा आरम्भ किये गये कुष्ठ-निवारण-कार्यक्रम की एक अन्य प्रमुख ऐतिहासिक घटना है सन् १९७५ में लक्ष्मणझूला कुष्ठ-बस्ती में औषधालय की स्थापना। इससे उन रोगियों को बहुत आराम प्राप्त हुआ जिन्हें इससे पूर्व आश्रम के चिकित्सालय तक का पूरा मार्ग चल कर आना पड़ता था। इन सब विकासों तथा सुधारों के होते हुए भी स्वामी जी उनकी दशा को और भी सुधारने को उत्सुक हैं। उनका भयंकर रूप से अपर्याप्त पोषण स्वामी जी के ध्यान का मुख्य केन्द्रबिन्दु बना हुआ है; क्योंकि इसके सुधार के अभाव में भारत के पचास लाख कुष्ठरोगियों के भाग्य में कोई वास्तविक ठोस परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो सकता है। निस्सन्देह उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही दिव्य जीवन संघ प्रति वर्ष सहस्रों रुपये व्यय करके स्थानीय कुष्ठ-बस्तियों के बन्धुओं को स्मरणीय लोकोपकारी सेवा प्रदान करने में सक्षम हुआ है।
स्वामी जी की कुष्ठियों की सेवा उनकी दिव्य प्रकृति की सुन्दर अभिव्यक्ति है। स्वामी जी, जो कि दिव्य जीवन संघ के परमाध्यक्ष तथा वर्तमान समय के महत्तम आध्यात्मिक नेताओं में से एक हैं और जो दर्शन तथा पथप्रदर्शन के लिए सभी सामाजिक स्थिति तथा व्यवसाय के अनेक भक्तों से सदा घिरे रहते हैं, दीनों में से सर्वाधिक दीनों से मिलने, उनमें से प्रत्येक के साथ कुछ प्रिय वचन बोलने तथा उनकी शारीरिक सुख-सुविधा की देख-भाल करने के लिए किसी-न-किसी तरह समय निकाल ही लेते हैं। गिरिधारी की कहानी जिसके लिए इतिहास सम्भवतः स्थान न दे सके; किन्तु यह लोकोपकारवाद के इतिहास में, सच्चे भाईचारे तथा स्वभाव-सौजन्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अभिलिखित होगी। गिरिधारी ढालवाला का एक निर्धन रोगी मात्र था। उसके हाथ की अँगुलियाँ नहीं थीं, नासिका न थी और न टाँगें थीं। उसकी पत्नी भी कुष्ठी थी। वह चलने-फिरने तथा अपनी जीविका के लिए भिक्षा माँगने में असमर्थ था। सभी लोगों ने उसे बहिष्कृत कर दिया था; किन्तु स्वामी जी ने उसे अपनी अचूक रक्षा प्रदान की। उस पर गुरुदेव की असीम कृपा थी और इसका कोई स्पष्ट विशेष कारण न था; किन्तु कष्ट जितना अधिक होता है, भगवान् तथा ईशमानवों की कृपा भी उतनी ही अधिक होती है।
स्वामी जी कदाचित् अपने प्रियतम शिष्य की जितनी देखभाल करते उससे भी अधिक उन्होंने गिरिधारी की की। बीस अथवा इससे भी अधिक वर्षों तक रोगी चलने में असमर्थ था और स्वामी जी इन सब वर्षों में उसे भोजन भेजते तथा सभी सम्भाव्य उपायों से उसकी देखभाल करते रहे। गिरिधारी सदा ही उनके ध्यान का प्रथम विषय # होता था। उदाहरणार्थ, वह जब अपनी लम्बी विश्व-यात्रा पर आश्रम से प्रस्थानविषय गाते थे तथा अपनी सकामनाएँ प्रदान करने वाले आश्रमवासियों से घिरे देने अकस्मात् उनका ध्यान उस बेचारे रोगी की ओर गया जिसके वह वर्षों तक परिचारक, पित्र तथा माता-पिता रहे थे। वह गिरिधारी की झोपड़ी में गये और यह गम्भीर वचन दे काउस विषण्ण व्यक्ति से विदाई ली कि वह उसे प्रतिदिन स्मरण करते रहेंगे। उस बेचारे ने करबद्ध प्रार्थना की तथा स्वामी से आश्वासन प्राप्त किया कि वह उसकी मृत्यु से पूर्व उसके पास अवश्य आ जायेंगे। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया, किन्तु उन्होंने उस दीन व्यक्ति को सदा अपने मन में बनाये रखा। वह सुदूर अमरीका से गिरिधारी की दरिद्र झोपड़ी को सर्वोत्तम उपलब्ध औषधियाँ तथा छोटे-मोटे उपहार समय-समय पर भेजते रहे।
जब गिरिधारी की मृत्यु अधिकाधिक निकट आ रही थी तो वह इस विचार से व्यधित था कि उसकी कई दशकों तक सेवा-सुश्रूषा करने वाले उसके गुरुदेव उसके अन्तिम दिनों में उसके पास नहीं हैं और सम्भवतः वह अपनी मृत्यु से पूर्व पूज्य गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पायेगा। ऐसे विचारों के कारण उसे अपने भौतिक शरीर से पूर्ण घृणा हो गयी और उसने भोजन लेना बन्द कर दिया। अपने शरीर को छोटे से कम्बल से ढक कर वह भूमि पर लेटा रहा। लोग सोचते कि वह मर चुका है। संयोगवश माता इवान लेब्यू ने उसे उस दुर्दशा में देख लिया। उन्होंने उसके जीवन को बचाये रखने का यथाशक्य प्रयास किया, पर रोगी इतना हठी था कि उसने सन्तरे अथवा अंगूर का रस भी लेना अस्वीकार कर दिया। किन्तु जब उसे यह बताया गया कि स्वामी जी शीघ्र वापस आने वाले हैं और यदि वह उनके दर्शन के लिए जीवित रहना चाहता है तो उसे कम-से-कम फलों का रस तो लेना ही पड़ेगा तो वह तुरन्त मान गया। माता लेब्यू ने स्वामी जी के अच्छी तरह चौखटा लगे हुए पुष्पमालयुक्त एक चित्र का प्रबन्ध किया। गिरिधारी पवित्र दर्शन के लिए प्रार्थना तथा अश्रुपात करता हुआ जागरण करता रहा। उस समय वास्तव में चमत्कार हुआ। उसकी प्रार्थनाएँ सुन ली गयीं। कोई भी यह विश्वास नहीं करता था कि स्वामी जी के आने तक गिरिधारी जीवित रह सकेगा। किन्तु ऐसा हुआ कि स्वामी जी नियत समय से ढाई माह पूर्व ही आश्रम वापस आ गये। जब उन्हें गिरिधारी की दशा का पता चला तो वह-जिन्होंने बीस वर्षों तक उसकी अथक सेवा-सुश्रूषा की थी-अब उसको शान्तिपूर्ण महाप्रयाण के लिए तैयार करने को उत्सुक थे। उन्होंने एक साधारण कम्बल खरीदा और ढालवाला में गिरिधारी की झोपड़ी में उससे मिलने गये। माता सिमोनेटा उस समय उसके पास उपस्थित थीं। स्वामी जी ने मृदु स्वर में गिरिधारी से कहा: "अब आप अपना शरीर त्याग सकते हैं। आप शान्ति से जा सकते हैं।" इस भाँति असीम करुणाशील गुरुदेव को अपने पास बैठा हुआ देख कर सद्भाग्यवान् गिरिधारी कुछ समय तक प्रसन्न तथा शान्त रहा और तत्पश्चात् उसने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उसे उसी छोटे सूती वस्त्र से ढक दिया गया और दिव्य नाम के उच्चार के साथ उसके शरीर का दाहसंस्कार किया गया।
असहाय लोगों के प्रति स्वामी जी की ऐसी हृदयस्पर्शी सेवा तथा प्रेम के उदाहरण अनेक हैं। ढालवाला का एक अन्य कुष्ठी जिसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली गयी थी, अपने दो बच्चों के साथ असहाय रह गया था। स्वामी जी को अपनी माँ से अलग होने पर बच्चों के दुःख तथा तत्परिणाम स्वरूप बेचारे पिता के कष्ट का पता चला। अतः वह उन बच्चों को आश्रम में लाये, उनको भोजन कराया तथा वस्त्र दिये और तत्पश्चात् उन्हें एक महिला चिकित्सक को समर्पित कर दिया जो उनकी माता जी बनीं। इस प्रकार के उदाहरण संख्यातीत हैं।
वर्ष में एक बार जब होली का आनन्दपूर्ण उत्सव आता है तब तीनों कुष्ठ-बस्तियों के कुष्ठी भाई प्रत्येक कुछ क्षणों के पश्चात् 'चिदानन्द भगवान् की जय' के तुमुल नाद के साथ नृत्य तथा गान करते तथा अपनी ढोलकै बजाते हुए आश्रम आते हैं। वे आते हैं, अपने मित्र तथा परित्राता से मिलते हैं और उस व्यक्ति को स्नेहमय नमस्कार करते हैं जो उनमें से प्रत्येक के जीवन में बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा है। इधर सन्त भी उनके समान उत्साह के साथ बाहर उनके पास आते, उनका स्वागत करते तथा उन्हें मिष्टान्न भेंट करते हैं। प्रेम तथा उल्लास, सन्त के मुख पर की कान्ति, कुष्ठियों के मुख पर की कृतज्ञता तथा स्नेह और पूर्णतया मुक्त तथा अबाध सत्कार-विनिमय दर्शकों में उन्नयनकारी आनन्दानुभूति संघटित करते हैं।
इस प्रकार उत्तराखण्ड की अभागी तथा पीड़ित आत्माओं ने स्वामी जी से शान्ति तथा आश्रय प्राप्त किया। सहानुभूतिशील स्वामी जी उन सबके न केवल चिकित्सक थे अपितु उनमें से प्रत्येक के स्नेहमयी माँ, कठोर पिता, सहायक मित्र तथा सर्वोपरि उद्धारक तथा परित्राता भी थे।
नवम अध्याय
महान् प्रबोधक
"य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ।।
--जो व्यक्ति मुझमें परम भक्तियुक्त हो कर मेरे भक्तगणों के मध्य में इस परम गुह्य शास्त्र की व्याख्या करेगा, वह मुझे अवश्य प्राप्त होगा, इसमें सन्देह नहीं है" (गीता : १८/६८) ।
"धैर्य रखें। निर्भीक बनें। मैं सदा आपके पास हूँ। मैं उस शाश्वत अन्तर्यामी से आत्मिक रूप में सदा अभिन्न हूँ और उसके अंश-रूप में मैं आपकी अन्तरात्मा में निवास करता हूँ।" यह चिदानन्द का समस्त भूमण्डलभर में फैले हुए उन असंख्य भक्तों के लिए भावप्रवण अभय वचन है जो उनके संरक्षण में असत् से सत् की ओर, तमस् से ज्योति की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर अग्रसर होने को संघर्षरत हैं। वह सार्वभौमिक मित्र, जगद्गुरु, अद्वितीय प्रेरक तथा सक्रिय दिव्य सन्देश वाहक हैं जो अपनी असीम अनुकम्पा, कान्तिमय शुचिता, भावपूर्ण भजन तथा आधुनिक युग के भौतिकवादियों के लिए विद्युत्-प्रघात-चिकित्सारूप गम्भीर चेतावनियों से मानव-जाति का भाग्य सुधार रहे हैं।
सन् १९४९ में गैरिक वस्त्र धारण करने तथा दिव्य जीवन संघ के महासचिव का पदभार लेने के समय से ही उन्होंने जनता को अकर्मण्यता तथा असावधानता से उद्बुद्ध करने तथा उन्हें उचित निर्णय करने तथा आत्मसाक्षात्कार के प्राप्त्यर्थ सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के बृहत्कार्य में अपने को पूर्णतया समर्पित कर दिया। एक महान् प्रबोधक के उनके व्यापक प्रयास की कहानी का आरम्भ कुछ साधारण रूप में हुआ। जैसा कि इससे पूर्व बतलाया जा चुका है, एक दिन शिवानन्द ने उन्हें बुला भेजा तथा दिव्य जीवन संघ की बिहार प्रादेशिक शाखा का उद्घाटन करने के लिए पटना जाने का आदेश दिया। यह केवल साधारण-सा सेवा-कार्य था जो संयोगवश उनके कन्धों पर लाद दिया गया था; किन्तु जनता पर इनके अभ्यागम का ऐसा आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा कि उसके बाद उन्हें विराम न उपलब्ध हो सका। समय की गति के साथ-साथ अधिकाधिक लोग उनके दयामय अवधान की जोरों से माँग करने लगे और तबसे वह भगवान् के भ्रमणशील सन्देशवाहक बने रहे।
स्वामी जी की पटना की यात्रा'[16] बिहार की सुविस्तृत यात्रा के रूप में समाप्त हुई। इसके पश्चात् उन्होंने गुरुदेव के साथ युगान्तरकारी अखिल भारत यात्रा की। सारे भारत के जिज्ञासु शीघ्र ही चिदानन्द की महत्ता को पूर्ण रूप से समझ गये। वे उनके धर्मोपदेशों तथा शिक्षाओं को अमूल्य वस्तु मान कर सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे। ऋषिकेश में सन् १९५३ में आयोजित 'विश्व धर्म परिषद्' के सभी अधिवेशनों में उन्होंने आदिप्रवर्तक की भूमिका अदा की। उन्होंने अपनी प्रत्ययकारी तर्क-शक्ति तथा तीव्र आध्यात्मिक उत्साह से श्रोताओं को यह मूलभूत सन्देश हृदयंगम करा दिया कि एकमात्र धर्म ही मानव-जाति में एकता ला सकता है। उन्होंने जनता पर जो प्रभाव अंकित किया उसको देख कर गुरुदेव ने जनता की आध्यात्मिक सेवा करने के लिए उन्हें अधिकाधिक बारम्बार बाहर भेजने की आवश्यकता अनुभव की। वही एक व्यक्ति थे जिन्हें वे विविध दिव्य जीवन सम्मेलनों की अध्यक्षता करने के लिए अपने निजी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सदा भेजते रहे।'[17]
जब कोलकाता में आठवाँ अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन हुआ उस समय स्वामी जी बदरीनारायण की तीर्थयात्रा पर गये हुए थे। गुरुदेव ने उन्हें नीचे बुला भेजा तथा जनता को उन्नत बनाने के लिए कोलकाता जाने का आदेश दिया। सम्मेलन में एकत्रित जिज्ञासुओं को 'नित्य पूर्ण, नित्य शुद्ध, आनन्दघन परमात्मा, सर्वशक्तिमान् अद्वय सत्ता के दृश्य व्यक्त रूप' कह कर सम्बोधित करने वाले उनके प्रथम शब्दों से ही पुलक की लहर वैसे ही दौड़ गयी जैसे विवेकानन्द के शब्दों से शिकागो की जनता में हुआ था। उनके शब्दों ने उतना नहीं जितना कि उन शब्दों में निहित सुष्पष्ट आध्यात्मिक शक्ति तथा भगवत्कृपा ने तत्काल भव्य प्रभाव उत्पन्न किया। गम्भीर, तेजस्वी तथा कुशाग्रमति स्वामी जी ने विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया कि दिव्य जीवन सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य लोगों के हृदय तथा मन में दिव्य भाव, आत्मिक एकता की उत्कृष्ट भावना, सर्वगत अभेद, भक्ति, भ्रातृभाव तथा प्रेम की तरंगें उत्पन्न करना है। सम्मेलन में कुछ भी संस्थागत विषय न था। उनका विचार था कि सम्मेलन को कलह तथा सम्भ्रम से विषाक्त आज के विश्व की एक भव्य नवीन रूप में कल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत करने में छलाँग लगाने के लिए एक फलक का रूप लेना चाहिए। यह (सम्मेलन) आध्यात्मिक उन्नति की ओर सतत अभिमुख नवीन मानवता प्रकट करने के लिए है।
स्वामी जी ने अपने उन्नयनकारी प्रवचनों में मानव-स्वभाव के निम्नतर, अशुद्ध तथा अहंकारी रूप को नष्ट करने तथा अन्तस्थित अपने उच्चतर दिव्य स्वरूप के साक्षात्कार करने में सहायता प्रदान कर उसमें उद्विकास लाने की आवश्यकता तथा उपायों को अपने श्रोताओं के मन में बैठाने के कार्य में स्वयं को लगाया। उनकी मान्यता के अनुसार ब्रह्माण्ड में सभी पदार्थ अपने सत्स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। एकमात्र मनुष्य ही अपराधी है। मनुष्य, जो कि ईश्वर-सृष्टि का मुकुट है, उसकी सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है, वैभवशाली विचार-शक्ति से सम्पन्न है, अपने स्वरूप में खरा नहीं है। आत्मोत्कर्ष में उसकी बुद्धि का दुरुपयोग होता है। उसने अपने को ऐन्द्रिक अन्तश्चालनाओं का दास बना डाला है तथा इस जगत् को शोक तथा परिताप की उपत्यका में परिवर्तित कर दिया है। ईश्वर के उद्यान को अपवित्र किया गया है। स्वामी जी ने सभी को स्पष्ट रूप से समझाया कि दिव्य जीवन कोई गुप्तोपासना नहीं है। उन्होंने कहा: “निस्स्वार्थता तथा आत्मसाक्षात्कार को, मानव-सेवा तथा ईश्वराराधन को ही दिव्य जीवन समझो।" उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह सम्मेलन इस सन्देश को श्री रामकृष्ण तथा विवेकानन्द की स्मृति से अभिषिक्त महानगर कोलकाता के ही नहीं अपितु विश्व के सभी भागों के प्रत्येक घर में पहुंचाये।
उनके जोशीले सन्देश ने कोलकाता की जनता पर अपना अमिट प्रभाव डाला जो कई वर्षों के बाद जब १९७४ में दिव्य जीवन सम्मेलन की रजत जयन्ती आयोजित की गयी, उस समय भी दिखायी पड़ता था। चिदानन्द द्वारा फहराये गये ध्वज के पास सहस्रों जिज्ञासु एकत्रित हुए। सीतारामदास ओंकारनाथ, वेदव्यासानन्द, शुद्धानन्द भारती तथा चिन्मयानन्द जैसे सन्तों ने स्वामी जी के प्रति अपने व्यक्तिगत प्रेम तथा सम्मान के चिह्नस्वरूप अपनी उपस्थिति से सभामंच को सुशोभित किया। ओंकार बाबा ने चिदानन्द को शिवानन्द का प्रकट रूप बतलाया तथा वेदव्यासानन्द ने उन्हें आधुनिक विवेकानन्द के रूप में चित्रित किया। स्वामी जी ने अपने प्रवचन में भगवत्साक्षात्कार के लिए संघटित चेष्टा पर बल दिया। उनका विचार है कि जीवन के किसी भी अंग से इस चेष्टा को कुण्ठित नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने दर्शाया कि किस प्रकार व्यक्ति की क्रिया का प्रत्येक अंश भगवान् की दिशा में एक पुरोगामी डगे बन सकता है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा : "इस जीवन का अस्वीकरण नहीं, वरन् इसका रूपान्तरण ही आज का युगधर्म है।"
स्वामी जी में लोगों की अभिरुचि की लहर बंगाल से गुजरात तक फैल गयी। दश वर्ष से अधिक समय तक उस (गुजरात) राज्य के विविध आध्यात्मिक सम्मेलनों में स्वामी जी आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन तथा सामाजिक सौहार्द लाने के कार्य में संलग्न रहे। इनका प्रभाव विशेषकर पाटण तथा राजकोट की जनता पर आश्चर्यकर रूप से पड़ा। उनके दिव्य व्यक्तित्व से द्वारका के जगद्गुरु शंकराचार्य तथा बाबा रणछोड़दास जैसे अन्य उन्नत आध्यात्मिक नेता उन समारोहों में आने को आकर्षित हुए। यह स्थिति स्वामी जी के सम्मेलनों में सदा ही होती है। जनता को दिव्य जीवन के प्रति सम्बुद्ध बनाने के लिए स्वामी जी न केवल स्वयं प्रयास करते हैं अपितु देश के अन्य लब्धप्रतिष्ठ सन्त पुरुषों की सद्भावनाओं की जो विपुल निधि उन्होंने संचित की है, उसका भी मुक्त रूप से उपयोग करते हैं।

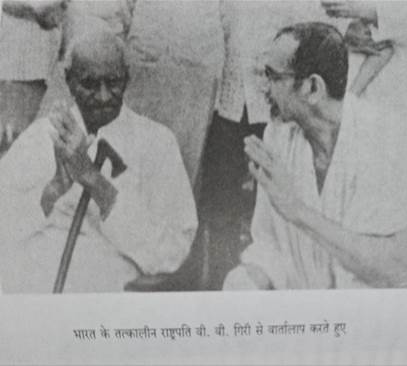
स्वामी जी को अपनी यात्राओं में प्राय: दिल्ली से हो कर जाना पड़ता है। वहाँ के भाग्यशाली भक्त जब कभी सम्भव हो उनके दर्शन तथा प्रवचन का लाभ उठाने के लिए सदा सतर्क रहते हैं। इन बारम्बार के सत्संगों का राजधानी तथा उसके अड़ोस-पड़ोस के भक्तों तथा जिज्ञासुओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।
स्वामी जी से उत्प्रेरित हो दिल्ली के भक्तों ने गुरुदेव की महासमाधि के कुछ ही महीनों के पश्चात् सोलहवाँ अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन आयोजित किया। स्वामी जी ने उन्हें यह महान् पाठ सिखाया कि गुरु कभी मरता नहीं तथा जहाँ तक भक्तों तथा जिज्ञासुओं का सम्बन्ध है, उन्होंने अनुभव किया कि गुरुदेव ने अपने चुने हुए उत्तराधिकारी के माध्यम से कार्य करना जारी रखा है। उन्हें 'स्वामी शिवानन्द सांस्कृतिक संस्थान' के आवास के एक भवन-निर्माण कराने और इस भाँति गुरुदेव की स्मृति को अमर बनाने की प्रेरणा मिली। स्वामी जी ने इसके उद्घाटन के अवसर पर डा. एस. राधाकृष्णन तथा न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोल्कर के साथ समारोह में उपस्थित हो उसकी शोभा बढ़ायी। जब वहाँ चौबीसवाँ अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन हुआ तो स्वामी जी ने श्रद्धेय ओंकार बाबा तथा अन्य लब्धप्रतिष्ठ भागवत पुरुषों के साथ उस पुण्य भवन को पावन किया। ऐसे अवसरों पर स्वामी जी ने राजधानी के सुविज्ञ प्रबुद्ध वर्ग पर अत्यधिक आध्यात्मिक प्रभाव डाला।
स्वामी जी सतरहवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए सन् १९६४ में प्रथम बार पंजाब गये। उनके इस अभ्यागम को भक्तजन अब भी एक असाधारण आध्यात्मिक शक्ति से अभिरंजित अभ्यागम के रूप में स्मरण करते हैं। स्वामी जी जब चण्डीगढ़ पहुँचे तो वह स्टेशन पर ही पवित्र सप्तसिन्धु क्षेत्र के लोगों के आध्यात्मिक जागरण के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु से हार्दिक प्रार्थना करते हुए कुछ समय निश्चल तथा अन्तर्मुखी स्थिति में खड़े रहे। सम्मेलन-स्थल पर पहुँच कर जब वह सभामंच पर जाने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो लोगों ने विस्मय तथा धर्मोत्साह के नवीन भाव से अपने को अनुप्राणित अनुभव किया। उन्हें वह एक उन्नत कोटि की तेजस्विता तथा प्रशान्ति से देदीप्यमान दिखायी पड़े। वातावरण तत्काल श्रद्धास्निग्ध भावना से प्रभारित हो चला। स्वामी जी ने मधुर स्मित तथा नमस्कार के साथ सबका अभिवादन किया। सबकी दृष्टि उन पर ही केन्द्रित थी। वह एक मिनट तक पूर्णतः अन्तर्मुखी हो मूर्ति की तरह निश्चल बैठे रहे। तत्पश्चात् जब उन्होंने ॐ का उच्चारण किया तो स्पष्ट रूप से शान्ति तथा नीरवता छा गयी तथा श्रोता मुग्ध-से हो गये। सम्मेलन के प्रथम दिन लगभग आठ सहस्र पुरुष तथा महिलाएँ वहाँ एकत्रित हुए थे। आगामी दिवस को भीड़ शीघ्र ही लगभग पन्दरह सहस्र तक बढ़ चली। वे सभी आनन्द कुटीर के सन्त की झाँकी पाने तथा उनका उन्नयनकारी धर्मोपदेश सुनने को उत्कण्ठित थे। सभी ने यह अनुभव किया कि स्वामी जी ने वहाँ जो आध्यात्मिक उत्साह उत्पन्न किया वह असाधारण रूप से प्रगाढ़ तथा अवर्णनीय रूप से प्रभावकारी था। अमृतसर के स्वामी निर्मल महाराज भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया था तथा इसकी चर्चा की थी।
इसी प्रकार सन् १९६५ में मैसूर'[18] अठारहवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन के मंच पर स्वामी जी की जनता के समक्ष उपस्थिति स्मरणीय है। गुरुदेव की ऐतिहासिक यात्रा के पन्दरह वर्ष पश्चात् स्वामी जी उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में दक्षिण भारत के सभामंच पर प्रथम बार पधारे थे। गुरुदेव के दक्षिण भारत के बहुसंख्यक भक्त, जो वहाँ गये हुए थे, यह देख कर कि चिदानन्द छरहरे तेजस्वी शरीर में शिवानन्द ही हैं, अभिभूत हो गये। यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी को उनके आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के उदात्त कार्य में पुरी तथा द्वारका के शांकर पीठों के शंकराचार्यों ने भी अतीव कृपापूर्वक अपना सहयोग प्रदान किया। मैसूर सम्मेलन के पश्चात् स्वामी जी ने इस राज्य में कई क्षेत्रीय सम्मेलनों में भाग लिया।
सन् १९७१ में अपनी त्रिवर्षीय विश्व यात्रा से भारत वापस आने के पश्चात् स्वामी जी ने आन्ध्र प्रदेश की राजधानी में बाईसवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन की पूर्व सन्ध्या को हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के नगर-द्वय की प्रमुख सड़कों पर दिव्य नाम के उच्च स्वर से संकीर्तन की संगति में अन्य सन्तों के साथ उनकी शोभा-यात्रा निकाली गयी। बहुत से सन्तों के अतिरिक्त लौकिक क्षेत्र से आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल महामहिम खण्डूभाई देसाई तथा जनरल करियप्पा जैसे अनेक लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति स्वामी जी की भावोत्तेजक प्रार्थना तथा उन्नयनकारी प्रवचनों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने जिज्ञासुओं से इस आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट रूप से समझने का अनुरोध किया कि ईश्वर पर हमारा दिव्य अधिकार है। उन्होंने समाह्वान किया : "आत्म-विस्मृति की निद्रा से जग जाइए। आपकी साधना केवल यही होनी चाहिए कि हम ईश्वर के साथ अपने मधुर सम्बन्ध को कभी विस्मरण न होने दें।" उच्च तथा स्पष्ट स्वर में उन्होंने घोषित किया: "ईश्वर सदा मुझमें है। मैं सदा ईश्वर में हूँ।" उन्होंने आगे कहा: "दिव्य होना तथा दिव्यतापूर्वक जीवन-यापन करना आपके लिए स्वाभाविक है। आपका जो स्वरूप है, वही बने रहें। अपने स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कुछ बनना अस्वीकार कर दें।"
हार्दिक अनुरोध तथा अनुकम्पा से सन्तृप्त सरल आप्त वाणी का श्रोताओं पर अमित प्रभाव पड़ा। श्रोताओं में से अनेक लोगों ने यह अनुभव किया कि स्वामी जी के आध्यात्मिक उपदेशों की वृष्टि केवल स्फूर्तिदायक तथा प्रोत्साहक ही न थी, उसने स्वामी जी की दिव्य कृपा का अपरोक्ष रूप से उनमें संचरण भी किया। स्वामी जी ने अपने समापन-भाषण में श्रोताओं को चेतावनी दी कि वे भगवत्साक्षात्कार हेतु प्राप्त इस दुर्लभ मानव-जीवन को व्यर्थ नष्ट न करें। स्वामी जी ने गम्भीर वाणी में कहा : “प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के साथ काल तीव्र गति से निकला जा रहा है। प्रत्येक क्षण व्यतीत होता जा रहा है। अतः सभी हर्षोल्लास अनुचित हैं। अपने-आपसे पूछें, 'एक वर्ष व्यतीत हो चला। मैंने क्या किया? दुर्लभ मानव-जन्म को प्राप्त कर मैं क्या कर रहा हूँ?' सागर की दिशा में प्रवाहित होना सरिता का स्वधर्म है; वैसे ही अपने मूल स्रोत से मिलना जीव का स्वधर्म है। स्वगृह को लौटना ही जीवात्मा का परम कर्तव्य है।"
सन् १९७५ के बेंगुलूरु सम्मेलन ने एक और स्मरणीय आध्यात्मिक सेवा प्रदान की। विश्वेश्वर तीर्थ, शिव बालयोगी तथा शुद्धानन्द भारती जैसे श्रद्धेय महात्माओं की संगति में स्वामी जी मंच पर असाधारण प्रभा से देदीप्यमान हो उठे। उन्होंने गुरुदेव के चित्र का अनावरण किया और इस अनावरण-विधि को मानव-हृदय में सदाचार तथा भारतवर्ष की योग-परम्परा के उद्घाटन का विशेष नाम दिया। उन्होंने कहा: "वह अद्वय सत्ता, जिसकी मानव-समूह अल्लाह, खुदा, आहुर्मज्दा, ताओ के रूप में, परात्पर के रूप में पूजा करता है, जिस सत्ता को नास्तिक लोग अस्वीकार करते हैं, एक महासागर है जिसमें सभी धार्मिक धाराएँ प्रवाहित होती हैं। उसकी ही महिमा इंजील, कुरान, ग्रन्थसाहब तथा वेदों में गायी गयी है। उसकी ही प्रार्थना-भवनों, गिरजाघरों, मसजिदों तथा मन्दिरों में पूजा होती है। किन्तु उसका सबसे विशाल मन्दिर तो मानव-हृदय है। वह सबमें व्याप्त, प्रविष्ट तथा अन्तर्व्याप्त है। वही हमारी सत्ता का मूल तत्त्व है।" स्वामी जी मानते हैं कि मोक्ष की कुंजी प्राणी मात्र पर करुणा रखना है। यह करुणा अपने चतुर्दिक् उगने वाले पौधों तथा घासों तक विस्तृत करनी चाहिए। हमें प्रेम और सेवा के लिए ही जीना चाहिए। दूसरे, जीवात्मा को विश्वात्मा की विरह-वेदना का अनुभव होना चाहिए। उसे आध्यात्मिक लालसा होनी चाहिए जो उसको मौन बैठने, जप करने तथा धर्मग्रन्थों का स्वाध्याय करने में प्रवृत्त करे। योग के सभी रूप इस लालसा की बाह्य अभिव्यक्तियाँ हैं। यह अभीप्सा बाजार में नहीं खरीदी जा सकती है। इसे तो केवल भगवान् तथा सन्त ही प्रदान कर सकते हैं।
स्वामी जी इस भाँति अपने हृदयग्राही प्रवचनों से जनता में आध्यात्मिक अभीप्सा उत्पन्न करते हुए भारतवर्ष के कोने-कोने तक परिव्रजन करते रहे। सन् १९६६ तक उड़ीसा छूट गया था। निस्सन्देह स्वामी जी ने सन् १९५६ में कटक की आकस्मिक यात्रा की थी। एक दशक के पश्चात् उन्होंने भगवान् जगन्नाथ की भूमि में पुन: पदार्पण किया। वह पुरी में द्वितीय चैतन्य महाप्रभु के रूप में आये तथा उन्होंने जगन्नाथ भगवान् के मन्दिर के परिसर में भावप्रवण तथा उन्नयनकारी कीर्तन किया। उन्होंने प्रथम अखिल उड़ीसा दिव्य जीवन सम्मेलन की अध्यक्षता की तथा जनता को दिव्य नाम की महिमा से अनुप्राणित किया। भावुक प्रेक्षकों को ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में शुचिता छा गयी। इसके पश्चात् स्वामी जी इस राज्य में अनेक बार आये, इसके भीतरी प्रदेश में भी दूर तक यात्राएँ कीं तथा वहाँ के लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का अभूतपूर्व प्रचार किया।
सन् १९६७ में उन्होंने कटक में द्वितीय अखिल उड़ीसा दिव्य जीवन सम्मेलन की अध्यक्षता की। वह पुनः पुरी गये और कहा कि वह जब-जब भी उड़ीसा आयेंगे, तो जगन्नाथ भगवान् के पवित्र मन्दिर में उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के सुअवसर का लाभ उठाना चाहेंगे। तत्पश्चात् वह ब्रह्मपुर में इक्कीसवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन की अध्यक्षता करने सन् १९६८ में पुनः उड़ीसा आये। प्रकाशम हाल, जो सभा-स्थान था, भक्तों तथा जिज्ञासुओं से खचाखच भरा हुआ था। वे सब स्वामी जी की झाँकी पाने को उत्सुक थे। अनन्य वृत्ति वाले लोगों ने देखा कि किस प्रकार स्वामी जी अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम के होते हुए भी सभामंच पर प्रायः सहज समाधि की अवस्था में निश्चल बैठे थे और श्रोताओं पर सुख, शान्ति तथा आनन्द विकिरण कर रहे थे। उन्होंने शिवानन्दाश्रम में अतीव सावधानीपूर्वक तैयार की हुई अमृतोपम औषधि का अपने मर्मस्पर्शी भजनों तथा प्रवचनों द्वारा श्रोताओं में अन्तः क्षेपण किया। इनका सम्मेलन का संक्षिप्त सन्देश था : "जीवन का प्रकाश गुरूपदेश है। जीवन की शक्ति भगवन्नाम है। जीवन में सफलता का रहस्य भगवद्विश्वास है। जीवन का आधार धर्म है। जीवन की सम्पत्ति सद्गुण है। सर्वोत्कृष्ट निधि भगवद्भक्ति है। शान्ति तथा परमानन्द की कुंजी ध्यान है। परम कृतार्थता का मार्ग दिव्य जीवन है। जो कुछ कहा गया है, उस पर विचार करें, उसके कार्य को भलीभाँति समझें, अपने दैनिक जीवन में उनका अनुसरण करें तथा इस भाँति सौभाग्यशाली बनें।
स्वामी जी सन् १९७१ की ग्रीष्म ऋतु में पुनः उड़ीसा आये। इस बार उनका अभ्यागम जनजातीय क्षेत्र भवानी पटना में हुआ। आगामी वर्ष में वह तेईसवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए कटक गये। उड़ीसा के सभी भागों से लगभग ५०,००० लोग तथा देश के विभिन्न कोनों से अनेक प्रतिनिधि इस महान् ज्ञान-यज्ञ में स्वामी जी का दिव्योपदेश श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। स्वामी जी ने आह्वान किया : "हे भारतवासियो! जागो तथा संसार को धन्य बना दो। भारतवर्ष की सांस्कृतिक परम्परा के भाग्यशाली उत्तराधिकारियो! अपने जीवन को भारत के त्याग तथा सेवा के ज्वलन्त आदर्शों की दीप्तिमान प्रभा बना दें। अपने को हमारे धर्म का सजीव मूर्तरूप बना दें तथा अपने में परम आत्मज्ञान के अनुवर्ती परोपकार के उदात्त सिद्धान्तों का आदर्श प्रस्तुत करें। भारतवर्ष की उदात्त संस्कृति आप तथा आपके समूचे जीवन से प्रतिक्षण तथा प्रतिदिन सजीव रूप से अभिव्यक्त हो। इस भाँति आपके द्वारा भारत ओजस्वी रूप से सजीव तथा जाग्रत क्रियाशील बने। आप भारत हैं।"
स्वामी जी धीरे-धीरे क्योंझरगढ़ जैसे और अधिक भीतरी स्थानों की ओर समाकृष्ट हुए। वह वहाँ दिव्य जीवन सम्मेलन की अध्यक्षता करने गये तथा उन्होंने वहाँ अपना धर्म का सन्देश दिया। उन्होंने कहा: "धर्म का अवितथ रूप से अनुसरण करें। धर्म की उद्घोषणा करें। धर्म से मानव-समाज को अमित उपकार तथा लाभ होता है। धर्म की पुकार का सारे देश में प्रसार हो।"
स्वामी जी बमकोई के ग्रामीण क्षेत्र में गये। वहाँ उन्होंने भोले-भाले श्रद्धालु ग्रामीण जनों को अतीव सरल तथा स्पष्ट शब्दों में सम्बोधित किया। उन्होंने कामना व्यक्त की कि गुरुदेव का प्रत्येक शिष्य नित्य-निरन्तर पुजारी बना रहे। उन्होंने जप का गूढ़ अर्थ समझाया तथा जिज्ञासुओं को सभी समय तथा सभी अवसरों पर दिव्य नाम का जप करते रहने को कहा।
जब स्वामी जी राउरकेला में अगले दिव्य जीवन सम्मेलन की अध्यक्षता करने गये, तो उन्होंने मानव के इस परम कर्तव्य पर बल दिया कि वह अपने अन्दर की दिव्यता को पहचाने तथा अपने दैनन्दिन जीवन में अपने में अन्तर्हित दिव्य गुणों को व्यक्त करे। आचरण शुद्ध रखें, सत्यवादी रहें, निरन्तर प्रभु का स्मरण करें तथा अपनी सभी प्रवृत्तियों को आध्यात्मिक रूप दें-यह उस नगर-क्षेत्र के व्यस्त लोगों के समाह्नान के उच्च तथा स्पष्ट स्वर थे, हार्दिक अनुरोध था।
अब चिदानन्द की वाणी पश्चिमी उड़ीसा के चेता-केन्द्र से प्रतिध्वनित होने लगी। स्वामी जी सत्ताईसवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मलेशिया से वायुयान द्वारा कोलकाता होते हुए सम्बलपुर पहुँचे। सम्मेलन-काल के चारों दिन लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके मुखमण्डल से विकिरण होने वाली चुम्बकीय आभा का दर्शन करने, प्रेरणादायिनी ज्ञान-गिरा को श्रवण करने तथा उनके साथ भावोत्तेजक कीर्तनों का गायन कर भावविभोर बनने के लिए सहस्रों की संख्या में उत्सुक जनता से सभा-स्थल ठसाठस भर गया। स्वामी जी ने जिज्ञासुओं को व्यावहारिक शिक्षा देते हुए प्रत्येक छोटे कार्य को आदर्श रूप में निष्पन्न करके स्व-कर्तव्य-सम्पादन के महान् सद्गुण पर बल दिया। बूंद-बूंद जल से ही महासागर बनता है; स्वधर्म तथा साधना का दैनिक अभ्यास जीवन को परमानन्द के सागर से आपूरित कर देता है-इन्हीं सारगर्भित विषयों का सन्देश उन्होंने सम्मेलन को दिया।
स्वामी जी आगामी अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन के लिए भुवनेश्वर पधारे। उन्होंने साधकों को अनुप्राणित करने वाला अपना सन्देश देते हुए कहा : "हाँ, मेरे प्रिय मित्रो! मैं आपसे यह स्पष्टतया कह देना चाहता हूँ कि धर्म की तुला मनुष्य के कर्म को न केवल उसके प्रार्थना-पाठ तथा मन्त्रोच्चार की मात्रा से और न केवल दीपों के जलाने, आरतियों के उतारने, घण्टियों के बजाने तथा ग्रन्थों के स्वाध्याय करने की मात्रा से तोलती है अपितु वह अपने हृदय में आश्रय दी हुई भावनाओं के स्वरूप से, अपने पड़ोसियों के साथ वार्ता करते तथा उन्हें सम्बोधित करते समय प्रयुक्त उसके शब्दों से तथा नियति ने जिन लोगों के साथ उसे अपना जीवन यापन करने का विधान कर दिया है उन सबके साथ उसके व्यवहार के प्रत्येक सामान्य कर्म से भी तोलती है।" भगवान् के इस दयाशील सन्देशवाहक ने अपने इन शब्दों में उस उद्देश्य का उद्घाटन किया जिसके लिए भगवान् ने हमें इस लोक में भेजा है।
स्वामी जी ने इन सभी मंचों से सनातन धर्म के व्यावहारिक अभिप्राय की विशिष्टताओं को उजागर करने का निश्चय कर रखा था। वह जनता को उन्नत करने तथा जिज्ञासुओं का पथ-प्रदर्शन करने के लिए सभी प्रकार की कठिनाइयाँ झेलने को तैयार थे। उन्होंने भंजनगर, भद्रक, राउरकेला तथा अन्य स्थानों के विभिन्न साधना-शिविरों में एक व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में उड़ीसा के जिज्ञासुओं की कृपापूर्वक सेवा की। उन्होंने अपनी उपस्थिति में खुर्दा रोड, जयपटना तथा बलांगिर के क्षेत्रीय सम्मेलनों को प्रोत्साहित किया। प्रत्येक स्थान में उनका प्रभाव अविस्मरणीय तथा प्रबल रहा है। उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम बी. डी. शर्मा इन सम्मेलनों से इतना अधिक प्रेरित तथा पुण्यीकृत हुए कि उन्होंने स्वामी जी से उड़ीसा के सचिवालय में आने तथा राज्य के लौकिक संव्यवहार का उत्तरदायित्व रखने वाले प्रशासकीय विभाग के कर्मचारी-वर्ग को प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया। स्वामी जी ने कुछ वर्ष पश्चात् सुनाबेडा-सम्मेलन से लौटते समय इस अनुरोध को पूरा किया।
जब परम पावन स्वामी जी ने अपने पार्थिव जीवन के साठ वर्ष पूरे कर लिए तथा उनके प्रेमी भक्तों ने इस अवसर पर एक उपयुक्त समारोह आयोजित करने की अनुमति की माँग की तो उन्होंने उनको गुरुदेव की तपोभूमि से भारतवर्ष की जनता को जाग्रत, शिक्षित तथा उत्प्रेरित करने के लिए एक साधना-सप्ताह तथा आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए परामर्श दिया। प्रोन्नत कोटि के आध्यात्मिक व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ायी तथा जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं तथा भक्तों को अपने बोधप्रद उपदेश दिये। श्री श्री माँ आनन्दमयी के आगमन से जयन्ती अपने चरमोत्कर्ष को पहुँच गयी। परम पावन स्वामी जी के साथ में उनके दर्शन ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।
स्वामी जी ने सामान्य रूप से मानव जाति को तथा विशेष रूप से भाग्यशाली भारतीयों को जाग्रत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है। उन्होंने भारतभर में अनेक सम्मेलनों द्वारा लोगों को जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति, दिव्य पूर्णता तथा जीव के वास्तविक तथा शाश्वत आन्तर सत्ता में प्रच्छन्न आत्मिक सौन्दर्य के प्रकटीकरण के प्रति नवीकृत बोध जाग्रत करने की सेवा की है। उन्होंने बद्ध जीवों तक ब्रह्माण्डीय प्रकाश का प्राचुर्य लाने के लिए उनके द्वारों को जोरों से खटखटाया है। उन्होंने आन्तरिक उद्घाटन तथा उसकी सक्रिय अभिव्यक्ति-इन दोनों के लिए कठोर श्रम किया है, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्यों ने इन्द्रियों की तुष्टि के अन्धानुसरण से अपने को जिस अस्तव्यस्तता तथा ससम्भ्रम की स्थिति में डाल रखा है, उसका उपयुक्त प्रतिकार प्रदान करते हैं। वह जब कभी भी उन आध्यात्मिक सम्मेलनों में से किसी में उपस्थित नहीं हो सके तो उन्होंने अपने सुदूर के शिविरों से ऐसी सभाओं की सफलता में गहरी रुचि ले कर साधकों को अचूक रूप से प्रोत्साहन तथा पथ-प्रदर्शन प्रदान किया। उदाहरणार्थ, बौध के आयोजक, जब उनकी अनुपस्थिति के कारण निरुत्साहित हो रहे थे, उन्होंने सुदूर जोहान्सबर्ग से उन्हें उत्कण्ठापूर्वक पत्र लिखा तथा अपने उत्कृष्टतम आशीर्वाद से विश्वास दिलाया कि भगवान् जगन्नाथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे तथा
उसे महान् सफल बनायेंगे। ऐसे सम्मेलन उस जड़ता को दूर करने के लिए आज की महान् आवश्यकता हैं जिसने मानव की चेतना को आच्छादित कर रखा है। स्वामी जी ने इनके माध्यम से लोगों को धर्म-पथ पर ले जाने के लिए एक विश्वव्यापी कार्यक्रम आरम्भ किया है। अत: यदि हमारे समसामयिक सन्त उन्हें एक उद्धारक मानने को प्रेरित हुए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
दशम अध्याय
असाधारण दिव्य व्यक्तित्व
"परोपकाराय सतां विभूतयः
-सज्जनों की सम्पत्ति परोपकार के लिए ही होती है।"
शिवानन्द जी ने मानव-जाति को जिस महत्तम निधि का उत्तरदान किया है वह है चिदानन्द जो उनके ही प्रतिरूप में ढले एक असाधारण आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनकी ही प्रतिकृति हैं। गुरुदेव अपने इस कथन में सुनिश्चित थे कि चिदानन्द अपने पूर्व-जन्म में एक उच्चकोटि के सन्त थे और उनका जन्म अपने इस अन्तिम जन्म में एक महान् कार्य पूर्ण करने के लिए हुआ है। गुरुदेव उनकी सर्वोपरि प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को यहाँ तक कहा - "आप सबको स्वामी चिदानन्द के साथ अपने गुरु के रूप में व्यवहार करना चाहिए। मैं भी अपने गुरु के रूप में उनका सम्मान करता हूँ। मैंने उनसे असंख्य शिक्षाएँ ग्रहण की हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ।" भविष्यवक्ता के इन शब्दों को अचिन्तित, अति-उदार प्रशंसोक्ति नहीं समझा जा सकता। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, स्वामी जी जो कुछ भी कहते अथवा करते रहे हैं उन सबके द्वारा उन्होंने अपने वास्तव में अद्वितीय होने का औचित्य अधिकाधिक सिद्ध किया है। वह सर्वथा विमल दिव्य जीवन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जिस प्रकार गुरुदेव उनसे अत्यन्त प्रभावित थे उसी भाँति अन्य सन्त भी स्वामी जी की उच्च आध्यात्मिक स्थिति से प्रभावित हुए हैं।
कहा जाता है कि नित्य सिद्ध आत्माएँ मानव जाति का पथ-प्रदर्शन करने के लिए समय-समय पर भूलोक में अवतरित होती रहती हैं। भगवान् की कार्य-विधि अबोधगम्य है; इसी भाँति ईश-मानवों की भी कार्य-विधि अबोधगम्य हुआ करती है। अपने क्षुद्र अहं से आबद्ध हम कठिनाई से समझ सकते हैं कि वे क्या थे और वे क्या हैं। पाश्चात्य देशों में अनेक लोग स्वामी चिदानन्द पर भारत के सन्त फ्रान्सिस के रूप में श्रद्धा करते हैं। असीसी के सन्त फ्रान्सिस की सरल प्रार्थना, जो स्वामी जी का प्रिय स्तुति-गीत है, निश्चय ही वह आदर्श है जिस पर उनके जीवन का निर्माण हुआ है। अन्य कुछ लोग उनके भावप्रवण संकीर्तनों तथा सार्वभौम प्रेम के कारण उन्हें श्री चैतन्य के अवतार के रूप में पूज्य मानते हैं। स्वामी जी का हृदय बुद्ध के हृदय की भाँति कोमल तथा प्रफुल्ल है। वह पीड़ित प्राणियों को देखते ही द्रवित हो जाता है तथा गम्भीर सहानुभूति और व्यग्रता से उनके पास जाता है। इनकी चिन्ता का विस्तार वनस्पति-जगत् तक है। महाशिवरात्रि के दिन आश्रम के भक्तजन भगवान् शिव की पूजा के लिए जब बिल्वपत्र एकत्र करने जाते हैं तो उन्हें यह परामर्श देते हैं कि वे वृक्ष की ओर कुल्हाड़ी उठाये हुए न जायें; क्योंकि इससे वृक्ष भयभीत हो जायेगा। वे वृक्ष के पास स्नेह तथा विनम्रतापूर्वक जायें और उससे पत्तियों के लिए याचना करें। पत्ते तोड़ने का कार्य कोमलता, प्रेम तथा भक्तिभाव से करें।
स्वामी जी की आन्तरिक स्थिति वर्णनातीत है। स्वामी वेंकटेशानन्द के शब्दों में, "उनका वर्णन करने का प्रयास न करें। आप असफल रहेंगे। मौन भगवान् का नाम है।"
एक बार राउरकेला में सभामंच पर जब उनका परिचय 'एक असाधारण दिव्य व्यक्ति' के रूप में दिया गया तो उन्होंने अपने भाषण के प्रारम्भिक भाग में कहा कि यदि श्रोताओं में से प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करे कि वह भी एक दिव्य व्यक्ति है तो 5/4 * 3/4 सम्मान को स्वीकार करता हूँ। यह निश्चय ही उनके जन्म के उद्देश्य को व्यंजित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान् ने चिदानन्द को हमें यह निश्चय कराने के लिए भेजा है कि जैसा सत्त्व उनमें है, वैसा सत्त्व-सम्पन्न व्यक्ति मर्त्य मानव मात्र नहीं समझा जा सकता है।
चिदानन्द गुरु-भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। गुरुदेव के समस्त उच्चतर गुणों से सम्पन्न होने पर भी इस महान् आत्मा ने केवल एक समर्पित शिष्य की भूमिका अदा करना ही पसन्द किया है। वे अपनी सभी महती नैतिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों का श्रेय विनम्रतापूर्वक गुरु-कृपा को ही देते हैं। वे जो कुछ करते हैं, वे जो-कुछ भी कहते हैं वह सब वे सदा ही गुरुदेव शिवानन्द के नाम से ही करते हैं। यह अहंभाव के पूर्ण उन्मूलन तथा गुरु के प्रति अशेष आत्मसमर्पण का उत्कृष्ट निदर्शन है। उन्होंने गुरुदेव के जीवन-काल में अपने एक प्रेरणादायी प्रवचन में बल दिया: "गुरु भगवान् के समान नहीं है, गुरु भगवान् ही हैं।" एक अन्य प्रवचन में उन्होंने श्रद्धामयी कृतज्ञता के साथ अपना उद्गार प्रकट किया: "पूर्व-जीवनों के अनन्त पुण्यों ने हमें इस पवित्र स्थान में बैठने तथा उस अपरिमित आध्यात्मिकता की, अपरिमित दिव्यता की जीवन्त ज्वाला से निःसृत अग्नि का दर्शन करने का यह उत्कृष्ट सुअवसर प्रदान किया है जिसे गुरुदेव ने अपने में मूर्तरूप दिया है।" यद्यपि स्वामी जी स्वयं एक अत्युच्च कोटि के प्रबुद्ध योगी तथा आधुनिक जगत् की आवश्यकताओं का समाधान प्रस्तुत करने को उत्कृष्ट रूप में उपयुक्त हैं; किन्तु वह कभी भी अपने ऊपर सन्त की कोई भी पदवी प्रक्षेपित करना नहीं चाहते हैं तथा अपने प्रत्येक कर्म को गुरुदेव के पवित्र चरणों में समर्पित कर पवित्र बनाते हैं। वह कभी भी ऐसा अनुभव नहीं करते कि वह गुरुदेव की गद्दी के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। वह सदा ही अपने को गुरुदेव के सेवक के रूप में ही निर्दिष्ट करते हैं। गुरुदेव के उत्तराधिकारी की हैसियत से, संस्था के अध्यक्ष के रूप में दिव्य जीवन संघ की शाखाओं की सम्बद्धता के प्रमाण-पत्रों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करते समय भी वह ऐसा ही करते हैं। वह कई बार विश्व की यात्राएँ कर चुके हैं, सनातन धर्म का सन्देश ले कर भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक परिभ्रमण कर चुके हैं। उन्होंने इतनी प्रशस्तियाँ तथा बधाइयाँ प्राप्त की हैं जितनी कि अन्य इने-गिने व्यक्तियों ने ही प्राप्त की होंगी। अगण्य जिज्ञासुओं ने अपने जीवन के एकमात्र आनन्द के रूप में इनकी कल्याणकारी कृपा का आश्रय लिया है। इन सबको वह गुरुदेव के चरण-कमलों में सहज भाव से अर्पित करते हैं। इनका कथन है कि 'भक्त जिस भगवान् की उपासना करता है वह कम-से-कम कुछ अंशों में उसकी कल्पना पर आधारित होता है, किन्तु उसका गुरु तो शरीर (की दृष्टि) से उपस्थित है। शिष्य अपने सद्गुरु की पूजा करता है और इस भाँति वह अन्ततः गुरु-भक्ति को यथार्थतः भगवद्भक्ति में रूपान्तरित करने में सफल होता है।'
स्वामी जी ने किसी आचार्य के चरणों के पास बैठ कर उपनिषदों का आद्योपान्त अध्ययन कभी भी नहीं किया। उन्होंने गुरुदेव से भी उनका अध्ययन नहीं किया। तथापि गुरुदेव ने उनके सम्बन्ध में कहा : "यद्यपि स्वामी चिदानन्द ने उपनिषदों का परिशीलन नहीं किया है और न वह उनका परिशीलन करना चाहते ही हैं, पर यदि आप उनके प्रवचनों को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उनमें समस्त औपनिषदिक ज्ञान स्पष्ट किया गया है। वह उपनिषदों को अपने हृदय से प्रकट करते हैं। वह ब्रह्मसूत्र तथा गीता के मूर्तरूप हैं।" स्वामी जी ने १९६४ के साधना-सप्ताह में 'मेरा ब्रह्मसूत्र' पर प्रवचन किया। अपने इस बोधप्रद प्रवचन में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिष्य के लिए गुरु-वाक्य ही ब्रह्मसूत्र है। ऐसा कह कर उन्होंने गुरुदेव-रचित एक पुस्तक निकाली और उसमें से एक परिच्छेद पढ़ कर सुनाया जिसमें वेदान्त का सार समाविष्ट था।
इस भाँति स्वामी जी अपने अनुकरणीय जीवन द्वारा यह शिक्षा देते हैं कि एक साधक को गुरुभक्ति-रूप कवच के द्वारा सदैव सुरक्षित रहना चाहिए। उनके उनतालीसवें जन्म-दिवस पर शिवानन्दाश्रम के सभी वरिष्ठ साधकों ने जब इन पर अपनी प्रशंसाओं की वृष्टि की तो स्वामी जी ने कहा, "आप सभी मूर्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका श्रेय तो मूर्तिकार को है। मूर्ति में मूर्तिकार की ही बौद्धिक क्षमता तथा प्रतिभा दृष्टिगोचर होती है। आप मूर्तिकार के विषय में सब-कुछ विस्मरण कर मूर्ति के विषय में सभी प्रकार की बातें कर रहे हैं। मूर्तिकार स्वामी शिवानन्द जी महाराज में विद्यमान है। स्वामी चिदानन्द के दिव्य अभियन्ता स्वामी शिवानन्द हैं। सभी गुणगान उन चरण-कमलों को ही उचित है।" स्वामी जी ने इससे यह दर्शाया कि व्यक्ति को किस प्रकार नाम तथा यश सहित अपने सभी कर्मों के फल को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। वह साधना के इस अत्यावश्यक विषय के प्रति हमारा ध्यान और आगे आकर्षित करते हैं कि साधक को इस नामरूपात्मक जगत् में सृष्टि के सौन्दर्य का अवलोकन करते समय सृष्टिकर्ता को सदा स्मरण रखना चाहिए।
उनके एक अन्य मंगलमय जन्म-दिवस के अवसर पर समारोह में भाग लेने के लिए कैलास-आश्रम के हरिहर तीर्थ जी महाराज शिवानन्दाश्रम पधारे। उन्होंने अपने प्रवचन में स्वामी जी की सेवाओं, आध्यात्मिक उपलब्धियों, उदारता तथा गुरु-भक्ति की प्रशंसा की। अपने उत्तर में स्वामी जी ने तीर्थ जी महाराज के प्रति उनके स्नेहमय शब्दों के लिए कृतज्ञता के गम्भीर भाव व्यक्त करने के साथ ही कहा, "मुझ पर की गयी प्रशंसा की वृष्टि तो गुरुदेव पर ही की जानी चाहिए। मैं तो उनका निमित्त मात्र हूँ। यदि परिपक्व फल मधुर है तो इसका कारण उसका बीज है। आज मैं जैसा तथा जो कुछ भी हूँ, वैसा मुझे गुरुदेव की कृपा ने ही निर्मित किया है।"
उड़ीसा के भद्रक नगर के एक साधना-शिविर में एक सच्चे जिज्ञासु ने यह जानने की अभिरुचि प्रदर्शित की कि क्या स्वामी जी अब भी किसी भावातीत लोक में गुरुदेव के दर्शन करते हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि उनके विषय में श्री गुरुदेव के दर्शनों का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हें प्रतिक्षण यह अनुभव तथा प्रत्यक्ष बोध होता है कि गुरुदेव उनके भीतर हैं, उनके बाहर हैं तथा आकाश के अणु-अणु में व्याप्त हैं।
स्वामी जी के पाश्चात्य जगत् के एक शिष्य डान ब्रिडेल ने उनसे अपना परिचय देने को कहा। इस पर स्वामी जी ने अपने कक्ष के अन्तिम छोर में वेदी पर प्रतिष्ठापित स्वामी शिवानन्द के एक चित्र की ओर इंगित कर दिया। तत्पश्चात् उन्होंने स्पष्ट किया कि जब गुरुदेव से यही प्रश्न किया जाता था तो वह प्रश्नकर्ता को दिव्य आत्मा अर्थात् अन्तरस्थ भगवान् की ओर निर्दिष्ट किया करते थे। डान ब्रिडेल ठीक ही कहते हैं: "यह स्पष्ट है कि शिवानन्द अपनी दिव्य सत्ता में निरवशेषीकृत हो चुके थे और स्वामी चिदानन्द शिवानन्द नामक उस दिव्य सत्ता को इतना पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित हैं कि उनका शिवानन्द के परम तत्त्व के साथ पूर्ण तादात्म्य हो चुका है।"
स्वामी जी अपने को शून्य तक हस्वीकृत कर अपने को तुच्छ समझने को सदा ही प्रयत्नशील रहते तथा अपने गुरुदेव के गुणगान के लिए सतत दृढ़संकल्प हैं। किन्तु उनकी-जैसी प्रभा किसी भी उपाय से गुप्त नहीं रखी जा सकती थी। 'किम्बर्ली' के इस अमूल्य रत्न, जिसे शिवानन्द ने अपने मिशन के कोहनूर के रूप में खोज निकाला था, की नियति में विश्व के महत्तम तथा श्रेष्ठतम लोगों से श्लाघा तथा सम्मान प्राप्त करना था।
"मैं प्रच्छन्न हीरा था;
प्रखर रश्मियों ने मुझे उद्घाटित कर दिया।"
जब व्यक्ति स्वामी चिदानन्द के विषय में चिन्तन करता है तो कुरानशरीफ के उपर्युक्त सारगर्भित शब्द उसे सहज ही स्मरण हो उठते हैं।
भले ही एक व्यक्ति इस भागवत पुरुष का विविध दृष्टिकोणों से अवलोकन करे, उसे इनके कार्यों में कुछ चमत्कारिक वस्तु अवश्य ही दिखायी पड़ेगी। वेदान्त-ज्ञान के उन्नत शिखर से संसार के गतिमान परिदृश्य को देखते हुए शान्त तथा अनुद्विग्न रहते हुए भी किसी जिज्ञासु आत्मा से मिलने पर वह एक संवेदनशील, स्नेही माता-पिता का कर्तव्य अपना लेते हैं। वह अपने लिए कठोरतम रूप के उपवास, तपश्चर्या, आत्मत्याग तथा संयम निर्धारित करते हैं तथा दूसरों को वह स्नेहिल अनुरोध, भ्रातृवत् अनुराग तथा मातृसुलभ देखभाल प्रदान करते हैं। उनका अविरत तथा सुसंगत लोकोपकारवाद अगण्य अवसरों पर प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुआ है।
एक बार स्वामी जी सन् १९७१ में महाशिवरात्रि के दिन सम्बलपुर गये। यह दिन अनेक कार्यक्रमों से संकुल था। यद्यपि उस दिन वह उपवास-व्रत रखे हुए थे, किन्तु उन्हें एक क्षणभर के लिए विराम प्राप्त नहीं हो सका। आगामी दिन प्रातःकाल उन्हें राउरकेला जाना था। उन्होंने एक भक्त के अनुरोध पर सम्बलपुर के निकट विश्वविख्यात हीराकुण्ड बाँध का चक्कर लगा कर जाने की बात स्वीकार कर ली। मार्ग में एक व्यक्ति कार को रोकने के लिए अपना हाथ हिला रहा था। कार-चालक उत्तर देने की मनःस्थित में न था। स्वामी जी उस समय कुछ कागज पढ़ रहे थे। उनकी सरसरी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने अनुभव किया कि कुछ गड़बड़ है और चालक को गाड़ी रोकने को कहा। वह गाड़ी से बाहर आ गये। बात यह थी कि वहाँ एक व्यक्ति घायल हो कर पड़ा था और यही कारण था कि वह व्यक्ति गाड़ी रोकने का प्रयास कर रहा था। स्वामी जी तुरन्त उस व्यक्ति के पास दौड़ कर गये, वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ कर घाव पर बाँध दिया और उसे गाड़ी में लाये। उन्होंने चालक को निकटतम चिकित्सालय को चलने के लिए आदेश दिया और आहत व्यक्ति के पास बैठ गये और इस बात को सुनिश्चित किया कि उसे यथासम्भव आराम मिल सके। उन्होंने उस व्यक्ति को बरला के चिकित्सालय महाविद्यालय के चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया और वहाँ से तभी प्रस्थान किया जब परिचर्या करने वाले चिकित्सक ने यह वचन दिया कि जब तक आवश्यक होगा वह उस आहत व्यक्ति के पास ही रहेगा। बाद में स्वामी जी ने कार के अपने सह-यात्रियों की घायल को देखने के तुरन्त बाद ही कार न रुकवाने के लिए शान्तिपूर्वक भर्त्सना की। "जरा अनुमान तो करो कि यदि हम ऐसी दुर्घटना के शिकार हुए होते तो हम कैसा अनुभव करते! हम घायल मित्र की उपेक्षा कर अपने कार्य के लिए कैसे आगे जा सकते थे?" ऐसे बहुसंख्यक उदाहरण हैं।
स्वामी कृष्णानन्द जी ने अपनी पुस्तक 'लाइट फ्राम द ईस्ट' में इसी प्रकार की एक घटना का उल्लेख किया है। वह लिखते हैं:
"एक बार स्वामी जी आश्रम के अपने दो सहयोगियों के साथ टैक्सी में यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्हें सड़क पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला जिसका सारा शरीर क्षत-विक्षत हो चला था। टैक्सी चालक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता रहा, किन्तु स्वामी जी ने शीघ्र ही उस दृश्य को देख लिया तथा चालक को गाड़ी रोकने को कहा। वे सब गाड़ी से उतर पड़े। पूछने पर पता चला कि वह व्यक्ति किसी दुर्घटना से घायल हो कर असहाय अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है। श्री स्वामी जी तुरन्त ही रोगी को उठा कर गाड़ी में रखने को तैयार थे जिससे कि उसे निकटतम चिकित्सालय में पहुंचाया जा सके, किन्तु चालक ऐसा नहीं करने देता था; क्योंकि उसे आशंका थी कि पुलिस इस विचार से कि उसकी गाड़ी से ही दुर्घटना हुई होगी, उसे अपराधी समझेगी और उसके लिए उसे उत्तरदायी ठहरायेगी। चालक उग्र था तथा अपनी गाड़ी में रोगी को ले जाने के किसी भी प्रस्ताव से सहमत नहीं होता था। स्वामी जी के लिए क्या विकल्प था? उन्होंने चालक को देय भाड़ा चुकता कर उसे चले जाने को कह दिया और स्वयं अपने दोनों साथियों के साथ उस रोगी को उठा कर निकटतम चिकित्सालय में, चाहे वह कितनी ही दूरी पर हो, ले जाने की तैयारी करने लगे। इस घटना की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। चालक का हृदय द्रवित हो गया और वह टैक्सी में रोगी को ले जाने के लिए सहमत हो गया।"
व्यक्ति अपनी निष्कपट निस्स्वार्थ सेवा से उद्दण्ड व्यक्तियों का हृदय सदा ही परिवर्तित कर सकता है। गुरुदेव ने अपनी पुस्तिका 'कर्मयोग-सम्बन्धी संकेत' में लिखा है कि 'किस प्रकार ऐसे सभी व्यवहार हृदय को पवित्र तथा विशाल बनाते, संकल्पशक्ति को सुदृढ़ करते तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मन को तैयार करते हैं।' स्वामी जी के लिए तो ऐसे कार्य उनकी बाल्यावस्था से ही उनकी प्रकृति के अंग बन चुके हैं। तथापि इस अवस्था में भी, जब वह आप्तकाम हैं और व्यक्तिगत साधना के रूप में उन्हें कुछ भी करने को शेष नहीं रहा है, वह इन व्यवहारों को केवल इसलिए बनाये नहीं रखते कि यह 'लोकशिक्षा' है तथा उनके शिष्य तथा प्रेमी उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे, वरन् इसलिए कि उत्कृष्ट कोटि की परोपकारिता का कोई परवर्ती- सामाजिक अथवा धार्मिक-उद्देश्य नहीं हुआ करता है।
इने-गिने सन्त ही स्वामी जी के समान मानव जाति की इतने विविध रूपों में सेवा करते होंगे। स्वामी जी ने मद्यपान जैसी बुराइयों के उन्मूलन के लिए एक उत्साही समाज-सुधारक की भाँति मूल स्तर पर कार्य किया है। उन्हें हतभाग्य मद्यपों पर दया आती है। वह उनके लिए प्रार्थना करते तथा उन्हें मदिरा-त्याग के लिए सहमत करने का प्रयास करते समय उन्हें अपमान करने का भी अवसर देते हैं। अपनी विश्व-यात्रा के समय एक बार जब वह ऐम्स्टर्डम में थे, एक अपराह्न में उन्होंने अपने साथियों से उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए कहा और चुपके से एक क्लब को चले गये जिसके विषय में उन्हें बताया गया था कि वह नगर के स्वापी व्यसनियों का सबसे बुरा अड्डा है। वह उसमें चुपके से घुस गये और उन सबको ध्यानपूर्वक देखा। उनके प्रति करुणा तथा सहानुभूति से अभिभूत हो वह तुरन्त ही उच्च स्वर से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपनी बुरी आदतों को त्याग देने के लिए उनसे करबद्ध प्रार्थना की। उनमें से कुछ लोगों ने उनके समीप जा कर उनका उपहास किया तथा बहुत ही अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कर उनसे निष्ठुरता से बातें कीं। उनमें से एक ने अपना शिरोवस्त्र उतार कर स्वामी जी के शिर पर पहना दिया। स्वामी जी प्रशान्त तथा निर्भीक रह कर उनके लिए प्रार्थना में प्रवृत्त रहे तथा मादक द्रव्य त्याग देने के लिए उनसे आग्रह करते रहे। प्रथम कुछ क्षणों के पश्चात्, उद्धत लोगों की कुछ कुचेष्टाओं के अनन्तर स्वामी जी द्वारा निःस्रावित निष्कपता तथा भावप्रवण प्रेम का आकांछित प्रभाव पड़ा। वह संकोच से शान्त हो गये। स्वामी जी ने उनसे कुछ बातें कीं। पुनः उनके लिए प्रार्थना की, उनकी मंगल-कामना की और वहाँ से विदा हो गये। अगले दिन उन व्यसनियों में से एक व्यक्ति अत्यधिक अनुतप्त तथा शुद्ध भाव से स्वामी जी के पास आया तथा उनके सत्संग में भाग लिया। वह स्वामी जी से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उस दिन से सभी मादक पदार्थों का सेवन त्याग दिया। उसने अन्य लोगों को बताया कि उन लोगों ने स्वामी जी के साथ कैसा रूखा व्यवहार किया था और स्वामी जी ने किस प्रकार उन सबको सहन किया तथा उनके कल्याण के लिए वह ईसा की भाँति प्रार्थना करते रहे।
स्वामी जी इस मदिरापान के महान् अभिशाप का हमारे देश से पूर्णतया उन्मूलन हुआ देखने को उत्सुक हैं। एक बार उन्होंने श्री सुन्दरलाल बहुगुणा की टिहरी की शराब की दुकानों पर धरना देने की योजना में उनकी सहायता करने को अपनी सेवाएँ अर्पित कीं। वह १ नवम्बर १९७१ को टिहरी से तीन किलोमीटर दूर दुबाटा पहुँचे और तत्पश्चात् सारे मार्ग में कीर्तन करते हुए टिहरी तक पाँव-पाँव गये। अब स्वामी जी ने मद्यनिषेध के आन्दोलन को आध्यात्मिक रूप दे डाला। शोभायात्रा के अन्त में, स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कहा कि पूर्ण मद्यनिषेध के लिए लिया हुआ कदम वस्तुतः सर्वशक्तिमान् प्रभु की पूजा ही है। उनके आशीर्वाद से सहस्रों सत्याग्रहियों ने शराब की दुकानों के दरवाजों पर धरना देना आरम्भ कर दिया और उनमें से अनेकों को कारागार भेज दिया गया। अन्त में उत्तर प्रदेश की सरकार उस क्षेत्र में मद्यनिषेध प्रवर्तित करने को बाध्य हो गयी। स्वामी जी कहते हैं कि दूषित वासनाओं वाले व्यक्तियों के लिए मोक्ष एक दूरस्थ स्वप्न है। उनके लिए तात्कालिक मोक्ष तो यही है कि उन्हें स्तेय, मदिरापान, मिथ्याचार तथा मिथ्यावादिता से दूर रखा जाय।
स्वामी जी की गुरुजनों के प्रति मर्यादा, महिलाओं के प्रति शिष्टाचार तथा बालकों के प्रति प्रेम सदा ही हृदयस्पर्शी होते हैं। व्यक्ति इनके सान्निध्य में कुछ दिनों रह कर इस विषय में अनेक शिक्षाप्रद कार्य देख सकता है। अपने लिए विशेष महत्त्वपूर्ण अवसरों पर भी वह दूसरों का विशेष लिहाज करते हैं। एक बार गुरुदेव का अभिनन्दन करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री की अध्यक्षता में दिल्ली नगर-भवन में एक सभा हुई। गुरुदेव भी इस समारोह में उपस्थित थे। स्वामी जी उस समय महासचिव थे। वह जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारा भवन खचाखच भरा हुआ है और अनेक महिलाएँ प्रवेश-द्वार पर सिमट कर बैठी हुई हैं। वह अपनी उपस्थिति की सूचना अथवा अन्दर प्रवेश करने के प्रयास द्वारा किसी को बाधा न डाल कर एक कोने में चुपचाप खड़े हो गये। जब एक प्रख्यात भक्त ने, जो उनके साथ-साथ चल रहा था, इनसे मंच पर आगे बढ़ने के लिए अनुरोध किया तो उन्होंने केवल इतना कहा- "मैं महिलाओं को बाधा पहुँचाना नहीं चाहता हूँ।" यह निश्चय ही एक छोटी-सी बात है, किन्तु स्वामी जी जैसे व्यक्ति के लिए कैसी सम्यक् है!
एक बार स्वामी जी गुण्टूर रेलवे स्टेशन पर थे। बहुत बड़ी संख्या में भक्तों ने उन्हें घेर रखा था। जब गाड़ी चलने को हुई तो वह उस डिब्बे में चढ़ गये जहाँ उनके लिए शायिका आरक्षित थी। जब गाड़ी चलने लगी तो उन्होंने प्लेटफार्म पर एक वृद्ध महिला को विलाप करते देखा। वह शोक कर रही थी कि वह अपना सामान बाहर नहीं ला सकी। स्वामी जी ने तुरन्त ही अपनी टोली के एक सदस्य को जंजीर खींचने के लिए कहा। गाड़ी रुक गयी। वृद्ध महिला ने अपना बोरिया-बिस्तर एकत्र कर लिया और प्लेटफार्म से प्रस्थान कर गयी। उसे यह पता न चला कि गाड़ी कैसे रुकी थी। स्वामी जी डिब्बे के द्वार पर खड़े थे और जब गार्ड इस विषय में पूछ-ताछ करने के लिए पहुँचा तो उन्होंने गार्ड को करबद्ध हो बुलाया और कहा- "कृपया मुझे क्षमा करें। उस वृद्ध महिला की विवशता देख कर मैंने ही जंजीर खींचने का आदेश दिया था।" उस कार्य विशिष्ट से कहीं अधिक शिक्षाप्रद थी उस अल्प समय में उनके व्यवहार की सम्पूर्णता-अकृत्रिम निष्कपटता, शिष्टता तथा दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। स्वामी जी के लिए यह समग्र विश्व एक विशाल परिवार है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने परिसर के सभी अन्य व्यक्तियों के लिए उत्तरदायी है।
इस भाँति एक अन्य अवसर पर जब स्वामी जी दिल्ली स्टेशन में उपस्थित थे, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन तथा आशीर्वाद के लिए एकत्रित हो गये। उमड़ती हुई भीड़ में उनकी दृष्टि एक वृद्ध महिला पर पड़ी जो अपने शिर पर भारी बोझ लिये तथा हाथ में एक सन्दूक पकड़े बड़ी कठिनाई से चल रही थी। स्वामी जी तुरन्त ही भक्तों को एक ओर कर उसके निकट तेजी से गये। उन्होंने उससे कोमल वाणी में कुछ कहा, उसके हाथ से भारी बोझ छीन लिया तथा उसे गन्तव्य स्थान तक ले जाने के लिए उसके साथ-साथ चलने लगे। तब स्वभावतः ही एक भक्त आगे आया और स्वामी जी के हाथ से सन्दूक ले लिया और उस वृद्ध महिला के लिए उसे ढोया। वैसे तो यह घटना भी बहुत ही साधारण-सी प्रतीत होती है; किन्तु सेवा करने के ढंग, सहज शालीनता, स्वाभाविकता तथा कार्य-सम्पादन की शिष्ट रीति ने इस कार्य को स्मरणीय बना डाला।
यह विश्व-मित्र ऐसा ही ध्यान पक्षियों, पशुओं, कीड़ों और यहाँ तक कि पौधों तथा लताओं का भी रखते हैं। उनका कहना है कि आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति की प्रगति उसके अधोवर्तियों, अधीनस्थों तथा छोटे नगण्य प्राणियों के साथ उसके व्यवहार से सहज ही मापी जा सकती है। उदाहरणार्थ कुत्तों को मारना केवल बालकों का ही नहीं, वरन् अनेक लोगों का एक प्रिय विनोद-सा बन गया है। स्वामी जी ने आश्रम में सबको बतला दिया था कि यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को पीटता है तो यह बात तुरन्त उनके ध्यान में लायी जाय। स्वामी जी ने जिस प्रकार महीनों तक प्रेम तथा ध्यानपूर्वक रोगी कुत्तों की सेवा की वह आश्रम में उनके प्रारम्भिक समय से ही एक लोकोक्ति बन गयी। वह उनकी सेवा तथा रक्षा करते तथा उनके लिए प्रार्थनाएँ करते हैं। एक बार वह कोलकाता में माता सावित्री नीलकण्ठ के अतिथि बने। सावित्री माता जी का सुन्दर बालों वाला एक मनोहर पालतू कुत्ता था। स्वामी जी के आने से कुछ माह पूर्व वह एक अचिकित्स रोग से पीड़ित था। उसके सब बाल झड़ गये और वह सूख कर काँटा हो गया। नगर में उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट औषधि के प्रयोग की रोग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सावित्री माता जी ने स्वामी जी से कुत्ते की दयनीय अवस्था की चर्चा की। स्वामी जी ने विस्तृत विवरण सुन कर कुत्ते को अपने पास लाने के लिए कहा। उन्होंने कुत्ते को अपनी गोद में बिठाया, कोमलता से उसे थपथपाया और जब वह उनकी गोद में लेटा हुआ था, उसके शीघ्र स्वास्थ्यलाभ के लिए महामृत्युंजय मन्त्र का जप किया। परिवार के सभी लोगों को आश्चर्य हुआ जब वह कुत्ता बिना किसी औषधि-प्रयोग के ही कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया।
इसी भाँति, एक बार जब स्वामी जी आश्रम में कीर्तन कर रहे थे तो एक अमरीकी दर्शनार्थी अन्दर आया और एक नन्हा सुकुमार पक्षी उनके सामने शान्तिपूर्वक रख दिया। उस पक्षी के पंख ताम्बूल-पत्र के सदृश्य थे। यह स्पष्ट था कि उसने बाहर कहीं से उसे अर्द्धमृतावस्था में उठाया था। कीर्तन समाप्त होने पर स्वामी जी की दृष्टि उस पक्षी पर पड़ी। विषाद तथा करुणा से आविष्ट गम्भीर वाणी में उन्होंने कहा, "आह! इसे कौन यहाँ लाया?" ऐसा कह कर उन्होंने उसे अपनी हथेली पर रख दिया तथा महामृत्युंजय जप करना आरम्भ कर दिया। पक्षी को मानो नया जीवन मिल गया और कुछ समय पश्चात् वह स्वच्छन्दता से उड़ गया।
बहुत बड़ी भीड़ में रहने पर भी वह इन बेचारे मूक प्राणियों की कठिनाइयों के प्रति सतर्क रहते हैं। एक बार जब उड़ीसा के बमकोई में एक आध्यात्मिक सम्मेलन चल रहा था, श्रोताओं में से किसी व्यक्ति ने एक कुत्ते को जो भीड़ में घुस आया था पीट दिया। स्वामी जी उस समय अपना अध्यक्षीय भाषण देने में तल्लीन थे। उन्होंने अकस्मात् भाषण देना बन्द कर उस निर्मम कार्य पर अपना मनस्ताप तथा कातर-भाव व्यक्त किया। श्रोताओं में गम्भीर निस्तब्धता छा गयी। स्वामी जी की वाणी में गूँजती हुई करुणा तथा मनस्ताप ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को स्पर्श किया। वह अपने विचार, वाणी तथा कर्म से न केवल "अहिंसा परमो धर्म:" के विख्यात नियम का सदासर्वदा अति-सावधानीपूर्वक पालन करते हैं अपितु उनके कर्म तथा आकांक्षा सर्वांशतः सकारात्मक रूप से करुणा से प्रभारित तथा दूसरों की व्यथा के उपशामन के प्रति निर्दिष्ट होते हैं।
उनका अहिंसा-धर्म खटमल तथा मच्छर जैसे छोटे-छोटे क्षुब्धकारी कीड़ों तक विस्तारित है जिन्हें लोग प्रायः प्रतिवर्ती क्रिया से मार डालते हैं और कुछ भी मनस्ताप नहीं करते। स्वामी जी उनके दंश को सहन करते हैं और उन्हें अपने शरीर के साथ मनमानी करने की छूट दे देते हैं। एक बार जब वह भगवन्नाम का कीर्तन कर रहे थे, एक शिष्य ने इनके शरीर पर एक मच्छर बैठा हुआ देखा और उसे भगा देने का प्रयत्न किया; किन्तु उसके उनके निकट आने से पूर्व ही स्वामी जी ने उसे संकेत से सूचित कर दिया कि वह उस प्राणी को बाधा न डाले। कीर्तन समाप्त होने पर स्वामी जी ने उससे कहा, "क्षुधित प्राणी अपनी क्षुधा तुष्ट करने के पश्चात् अपने-आप चला जाता है, आपको उसे भगाने की आवश्यकता नहीं है।"
इसी प्रकार की घटना कोटद्वार में हुई। जब स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, एक विषैला कीड़ा उनकी ओर उड़ा। उनके साथ के एक भक्त योगेश बहुगुणा जी ने तत्काल उसे भगा देने का प्रयास किया। स्वामी जी उस समय एक महत्त्वपूर्ण विषय पर बल देने में गम्भीरता से संलग्न थे; पर उनकी दृष्टि से यह ओझल न रहा। उन्होंने बहुगुणा जी को कीड़े को जाने देने का संकेत किया तथा अपना प्रवचन चालू रखा। कुछ समय पश्चात् उन्होंने दयालुता से कीड़े को उठा कर अपनी हथेली पर बिठा दिया मानो कि उसे पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हों। यह उस ज्ञानी की अद्वितीय ब्राह्मी-स्थिति है जो व्यवहार-जगत् के अपने व्यस्त कार्यक्रमों के होते हुए भी अहिंसा तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम के पालन के लिए सदा जागरूक रहता है। ऐसे उदाहरण असंख्य होंगे। लेखक ने उनमें से कुछेक का ही उल्लेख किया है जिन्हें उन अवसरों पर उपस्थित लोगों से सुनने का उसे संयोग हुआ है।
भक्तों की प्रार्थनाओं की पूर्ति करने का स्वामी जी का ढंग प्राय: चमत्कार की सीमा तक पहुँच जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब कभी भी भक्त पूर्ण निष्कपटता के साथ कोई भद्र संकल्प अपने मन में रखता है तो वह वैश्व-इच्छा से हो कर स्वामी जी तक स्वतः ही पहुँच जाता है। एक बार १९७४ की ग्रीष्म ऋतु में उड़ीसा के एक प्रख्यात भक्त प्रोफेसर चित्तरंजन महन्ती, जो आजकल दिव्य जीवन संघ पूर्वी क्षेत्र के महासचिव हैं तथा जिनका संन्यास-नाम (योगपट्ट) स्वामी शिवचिदानन्द है वालमोरिन में स्वामी विष्णुदेवानन्द के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के लिए कनाडा जा रहे थे। उनका विचार था कि उड़ान से पूर्व स्वामी जी का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ; किन्तु कोलकाता में उन्हें माता कमला चोपड़ा से पता चला कि स्वामी जी उस समय मुम्बई में हैं और कोलकाता में २६ मई तक आने का उनका कार्यक्रम है। इधर प्रोफेसर महन्ती को १६ तारीख को दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था। उन्हें यह जान कर अत्यधिक खेद हुआ कि वह अपने प्रस्थान से पूर्व स्वामी जी का दर्शन नहीं कर सकेंगे। अब सन्ध्या हो चुकी थी और वह अपने प्रस्थान में और अधिक विलम्ब नहीं कर सकते थे। उन्होंने महान् भक्त नरसी मेहता का विख्यात भजन "अब दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अँखियाँ प्यासी रे" एक कागज पर साश्रु लिखा जिसका अर्थ होता है- "हे मेरे प्रभु घनश्याम कृष्ण! मेरे नेत्र आपके दर्शनों के लिए प्यासे हैं। कृपा करके आप मेरे समक्ष प्रकट हों।" उन्होंने वह कागज पूज्य स्वामी जी को देने के लिए कमला चोपड़ा माता जी को दे दिया और तत्पश्चात् वह कोलकाता से प्रस्थान कर दिये। १८ तारीख को दिल्ली पहुँचने पर वह गुरुदेव के परम भक्त अमेरिकन इक्स्प्रेस के ए. सुन्दरम से मिले और उनसे अपनी मनोव्यथा व्यक्त की कि विदेश जाने से पूर्व वह स्वामी जी से नहीं मिल सकेंगे। और देखें! एक चमत्कार हुआ। श्री महन्ती को श्री सुन्दरम से यह सुन कर आश्चर्य हुआ, "हमारे साथ आइए। हम पालम हवाई पत्तन पर स्वामी जी का स्वागत करने जा रहे हैं। स्वामी जी ने अपनी कोलकाता की यात्रा निरस्त कर दी है और वह मुम्बई से सीधे दिल्ली आ रहे हैं।" व्यक्ति श्री महन्ती के अनिर्वचनीय आनन्द का सहज ही अनुमान लगा सकता है। वह श्री सुन्दरम तथा अन्य भक्तों के साथ हो लिये तथा उन्होंने हवाई पत्तन पर स्वामी जी का स्वागत किया। स्वामी जी ने उन्हें दिल्ली में अपने विश्राम-स्थल पर चलने के लिए कहा तथा उन्हें आश्वस्त किया कि जब प्रार्थना वास्तव में भावप्रवण होती है तो वह वैश्व मन में पहुँच जाती है और तत्काल स्वीकार कर ली जाती है।
एक बार बल्लारि में स्वामी जी एक भक्त के निवास स्थान पर अल्प काल के लिए गये। अपनी सामान्य रीति से प्रार्थना करने तथा प्रसाद वितरित करने के पश्चात् नगर के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वह वहाँ से शीघ्र ही चले गये। समारोह के पश्चात् जब वह अपने विश्राम-स्थल पर वापस आये तो उन्होंने कुछ ऐसी बात की जो विलक्षण-सी लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य को उक्त भक्त के घर से कुछ गरम दूध लाने के लिए उसके यहाँ भेजा। यह बात कुछ बहुत ही असामान्य थी और वह न केवल इसलिए कि स्वामी जी सामान्यतया कभी कोई वस्तु माँगते नहीं बल्कि इसलिए भी कि वहाँ पर ही प्रचुर मात्रा में दूध उपलब्ध था। तथापि शिष्य ने कुछ नहीं कहा और सहज भाव से स्वामी जी के आदेश का पालन किया। वह भक्त के घर गये तथा उन्हें स्वामी जी की इच्छा सूचित की। इस पर भक्त की पत्नी सहसा रो पड़ी तथा अपनी पाकशाला से दूध लाने के लिए भावावेश में दौड़ चली। भक्त ने स्पष्ट किया कि इससे पूर्व जब स्वामी जी प्रातःकाल उनके घर पधारे थे तब उसकी पत्नी उन्हें कुछ गरम दूध अर्पित करने को बहुत ही उत्सुक थी, किन्तु स्वामी जी के व्यस्त कार्यक्रम का विचार करके उसने ही स्वामी जी से ऐसी प्रार्थना करने को उसे दृढ़तापूर्वक मना कर दिया था। तथापि भाव ने अपना प्रभाव डाला तथा स्वामी जी ने यथासमय प्रतिक्रिया की। ऐसी बातें केवल संयोग प्रतीत हो सकती हैं; किन्तु घटना की बारम्बारता तथा रीति व्यक्ति को अन्य निष्कर्ष निकालने को विवश कर देती हैं।
अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना पर स्वामी जी की प्रतिक्रिया चमत्कारप्राय होती है। चतुर्थ अखिल उड़ीसा दिव्य जीवन सम्मेलन के अवसर पर स्वामी जी को विमान द्वारा भुवनेश्वर से भवानीपटना जाना था। दिव्य जीवन संघ की भुवनेश्वर शाखा के सचिव श्री राधाश्याम नन्दा ने स्वामी जी के स्वागतार्थ भुवनेश्वर में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की, किन्तु किसी कारणवश स्वामी जी की यात्रा के उत्तरदायी व्यक्तियों को कार्यक्रम की जानकारी न हो पायी थी और उन्होंने स्वामी जी को हवाई पत्तन पर विदा कर दिया। श्री नन्दा को निराशा हुई तथापि उन्हें देर तक मनस्ताप नहीं झेलना पड़ा। विमान आधी दूरी तक जा चुका था जब चालक ने यह कह कर विमान को पीछे की ओर मोड़ा कि आगे बुरा मौसम होने के लक्षण हैं। अतः विमान एक घण्टे के अन्दर ही भुवनेश्वर वापस आ गया। श्री नन्दा तथा अन्य भक्तों को, जो स्वामी जी के अकस्मात् प्रस्थान करने के कारण गम्भीर नैराश्य-भाव से खिन्न थे, यह जान कर चिन्ता से अत्यधिक राहत मिली कि वह वापस आ गये हैं। स्वामी जी सीधे सभास्थल को गये और अपना भाषण दिया, मानो कि वह उस कार्यक्रम के लिए ही आये थे। उन्होंने कार्यक्रम के अन्त में नन्दा जी से धीरे से कहा, "आपमें इतनी अधिक प्रगाढ़ भक्ति है कि भगवान् ने विमान को वापस आने को विवश कर दिया।" ऐसे रहस्यमय ढंग से उन्होंने भक्तों की उत्कट कामना की पूर्ति की।
गुरुदेव स्वामी शिवानन्द के एक प्रख्यात भक्त प्रो. दुर्लभचन्द्र चौधरी ने ग्रामवासियों को आशीर्वाद देने के लिए स्वामी जी को अपने जन्म-स्थान में आमन्त्रित किया। शीघ्र ही यह समाचार निकट के ग्रामों में फैल गया तथा जब स्वामी जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं तथा बच्चों सहित लगभग पाँच हजार लोगों की भीड़ मिली। वहाँ ध्वनिविस्तारक (माइक) की कोई व्यवस्था न थी; क्योंकि ऐसी बड़ी भीड़ का किंचित् भी पूर्वानुमान न था। दुर्लभ जी अत्यधिक चिन्तित हुए, किन्तु जब स्वामी जी दीर्घ स्वर से ॐ का उच्चारण करते हुए खड़े हुए तो उस अशिक्षित महिलाओं तथा बच्चों की भीड़ में असाधारण निस्तब्धता छा गयी। स्वामी जी ने सभा के पश्चात् दुर्लभ जी से यों ही कहा, "मैं आपकी विवशता को समझ गया था।" यह उनकी संकल्पशक्ति का स्पष्ट प्रमाण था।
प्रायः यह पाया गया है कि यदि महात्मा सिद्धियों का, प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाली असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करता है तो लोग उसे सिद्ध मानते हैं; किन्तु सच्चा सिद्ध, जिसने आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, अष्ट महासिद्धियों को रंचमात्र भी महत्त्व नहीं देता। वह अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में सदा स्थित रहता है। वह सन्तुष्ट, शोक रहित तथा करुणापूर्ण होता है। भगवद्गीता में अर्जुन ने भगवान् से जानना चाहा, "हे कृष्ण! समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण है? स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है?" भगवान् ने कहा, "हे अर्जुन ! जिस समय व्यक्ति मन में निहित समस्त कामनाओं को त्याग देता है तथा आत्मा से ही आत्मा में तुष्ट रहता है, उस समय वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। जिसका चित्त दुःख प्राप्त होने पर भी उद्विग्न नहीं होता, विषय-सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा नहीं रह गयी है एवं जिसके राग, भय तथा क्रोध निवृत्त हो गये हैं, वह मननशील व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जिसका पदार्थों में राग नहीं है, जो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर आनन्दित नहीं होता और न द्वेष करता है, जो राग, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जिसके इस मर्त्यलोक के सभी बन्धन छिन्न हो चुके है, जो सफलता से प्रसन्न तथा विफलता से खिन्न नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहते हैं।" चिदानन्द निस्सन्देह ऐसे ही स्थितप्रज्ञ हैं, त्रिगुणातीत हैं।
वह पद्मपत्र पर जल-बिन्दु की भाँति रहते हैं। वह सबकी सेवा करते हैं, किन्तु किसी से आसक्ति नहीं रखते हैं। उनमें समदृष्टि है, सन्तुलित मन है। वह भगवान् में स्थित हैं, अतः भगवान् उनके लिए सब-कुछ करते हैं। उनकी सभी प्रवृत्तियाँ भगवान् की, उनके विराट् स्वरूप में पूजा ही हैं। वे सूचित करती हैं कि वह न तो दुःख से क्षुब्ध होते हैं और न सुख से प्रहृष्ट। वह मानव मात्र पर सुख, शान्ति तथा आनन्द विकीर्ण करते हैं। संक्षेप में कहें तो वह इस हाड़-माँसमय शरीर में देवता हैं।
एक बार सन् १९७८ की ग्रीष्म ऋतु में लखनऊ के काल्विन तालुकदार महाविद्यालय के प्राध्यापक श्री के. के. वर्मा ऋषिकेश गये तथा बड़ी उत्सुकता से स्वामी जी को खोज निकाला। वह इस सन्त से कुछ विचारविमर्श नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि केवल स्वामी जी का दर्शन करने के लिए वह सारी दूरी तय करके आये हैं। उन्होंने स्वामी जी के परिचर को अपने आगमन की पृष्ठभूमि बतलायी। प्रख्यात सन्त-विद्वान् स्वामी चिन्मयानन्द सन् १९७७ में लखनऊ में अपने गीता-ज्ञानयज्ञ-काल में गीता पर शृंखलाबद्ध भाषण दे रहे थे। अपने प्रवचन में उन्होंने गीता-शास्त्र के आदर्श ईश-मानव, स्थितप्रज्ञ के लक्षणों का निरूपण किया। प्रो. वर्मा उनसे निस्सन्देह अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने प्रवचन के अन्त में चिन्मयानन्द जी के साथ साक्षात्कार की माँग की तथा उनसे सीधे प्रश्न किया, "क्या गीता का आदर्श स्थितप्रज्ञ एक श्रुतिविहित निरूपण मात्र है अथवा जीवन्त सत्य है? क्या भारत में आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उचित रूप से स्थितप्रज्ञ कहा जा सके?" बहुश्रुत संन्यासी जो सहज ही प्रशंसालु नहीं है, एक क्षण के लिए रुके फिर उन्होंने पूर्ण गम्भीरता तथा गुरुता से उत्तर दिया, "हाँ। ऐसे महात्मा हैं। एक माँ आनन्दमयी हैं और दूसरे स्वामी चिदानन्द हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन कर अपने को पवित्र बनाना चाहिए।"
उनके जीवन की असंख्य घटनाएँ सुख-दुःख, शीतोष्ण, लाभ-हानि, सफलता-असफलता तथा मानापमान में उनके मानसिक सन्तुलन को व्यक्त करती हैं। वह अपने व्यस्त कार्यक्रम में एक मूक साक्षी की भाँति तीनों गुणों के विलास को देखते हैं। एक बार जब वह वाल मोरिन में स्वामी विष्णुदेवानन्द द्वारा संचालित शिवानन्द-योग-वेदान्त-केन्द्र में थे तब विद्युत्-तन्त्र में लघु पथ के कारण उनके वासगृह में आग लग गयी। उनके देखने से पूर्व ही उसने विशाल ज्वाला का रूप ले लिया था। वह शान्तिपूर्वक वासगृह से बाहर आये तथा उस महाकक्ष के द्वार को खटखटाया जहाँ स्वामी विष्णु योग-वर्ग को प्रशिक्षण दे रहे थे। स्वामी जी को वहाँ खड़े देख कर स्वामी विष्णु को आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने उनसे अग्नि के लिए कुछ करने के लिए कहा; किन्तु विष्णु स्वामी ने स्वामी जी को ऐसी साम्यावस्था में पाया कि प्रथम तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और उसे उन्होंने एक परिहास समझा। किन्तु दूसरे क्षण ही उन्हें पता चल गया कि वह सच है और उन्होंने आग बुझाने के लिए आवश्यक पग उठाया। स्वामी जी का सभी आवश्यक सामान तथा अनेक महत्त्वपूर्ण अभिलेख अग्नि में नष्ट हो गये। तथापि वहाँ पर उपस्थित लोग यह देख कर आश्चर्यचकित रह गये कि इस सम्पूर्ण घटना-काल में स्वामी जी में विषाद अथवा चिन्ता का कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ। परवर्ती काल में जब उनसे प्रश्न किया गया कि उस समय उनका वास्तविक मनोभाव कैसा था तो उन्होंने कहा कि वास्तव में उन्हें दुःख का अनुभव हुआ, किन्तु वह दुःख उन दो स्नेही मकड़ियों के लिए हुआ जो उस कमरे में उनकी साथी थीं और जो ज्वाला में नष्ट हो गयी होंगी। क्या ही अतुलनीय करुणा ! क्या ही पूर्ण समचित्तता! गीता-प्रतिपादित स्थितप्रज्ञ वहाँ अपने में छोटे तथा बड़े सभी प्राणियों के लिए करुणाजनक एकमात्र शुद्ध संकल्प के साथ मध्यसागरवत् प्रशान्त, अनुद्विग्न खड़े थे।
एक बार स्वामी जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में रेलगाड़ी द्वारा कटक से जयपुर रोड (उड़ीसा) की यात्रा कर रहे थे। जब गाड़ी गन्तव्य स्थान पर पहुँची तो किसी ने उनके अताशे को स्मरण नहीं किया। गाड़ी के छूट जाने पर ही क्षति का पता चला। उस अताशे में अनेक मूल्यवान् कागज-पत्र तथा स्वामी जी के व्यक्तिगत उपयोग का सामान था। इससे साथ में जाने वाले भक्त इतना अधिक अशान्त हुए कि वे स्वामी जी के जयपुर (उड़ीसा) से क्योंझर का कार्यक्रम निरस्त करने को सोच रहे थे जिससे कार द्वारा रेलगाड़ी का पीछा करके अताशे को पुनः प्राप्त कर सकें; किन्तु स्वामी जी ने उनसे शान्तिपूर्वक कहा कि भगवान् ने उन्हें जो कार्य दे रखा है उसे निरस्त करना उनका कार्य नहीं है। उन्होंने स्वयं सुझाव दिया कि वे अगले बड़े स्टेशन के अधिकारी को दूरभाष द्वारा सन्देश मात्र भेज दें तथा प्रत्यासन्न कार्य की ओर ध्यान दें। उनकी क्योंझर की यात्रा के पश्चात् जब मण्डली बालेश्वर पहुँची तो अताशे स्टेशनमास्टर के पास सचमुच ही सुरक्षित मिला।
स्वामी जी को वहाँ से कोलकाता जाना था। मण्डली को स्टेशन जाने के मार्ग मैं एक उपरिपुल को पार करना पड़ा। समय हो गया था। अतः वे क्षिप्र गति से चल रहे थे। उनकी मण्डली के अन्य सदस्यों के प्लेटफार्म पर पहुँचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी; किन्तु स्वामी जी अब भी उपरिपुल के दूसरी ओर ही थे। जब कुछ भक्त उत्सुकतापूर्वक उन्हें खोजने के लिए भागे-भागे गये तो उन्होंने स्वामी जी को एक अन्धे व्यक्ति के पास पाया। बात यह हुई कि इस अन्धे व्यक्ति ने स्वामी जी से कुछ देने के लिए याचना की थी; किन्तु स्वामी जी उसे कुछ भी नहीं दे सके थे, क्योंकि उनका थैला पहले ही प्लेटफार्म पर पहुँच चुका था और स्वामी जी उसे कुछ दिये बिना जा नहीं सकते थे। उनके मिलने पर भक्तों ने उनसे कृपापूर्वक शीघ्र चलने की प्रार्थना की; क्योंकि गाड़ी किसी भी क्षण चल सकती थी। इस पर स्वामी जी ने अपना कुछ भी मत व्यक्त नहीं किया। उन्होंने अपना ऊपरी वस्त्र फैला दिया और उन सबसे उस अन्धे व्यक्ति की ओर से भिक्षा माँगी। भक्तों ने वस्त्र पर नोट तथा सिक्के डाल दिये। स्वामी जी ने उस सबको एकत्रित किया तथा उस बड़ी धनराशि को अन्धे व्यक्ति को दे दिया तथा उसके कान में गुप्त रूप से यह फुसफुसाया कि वह रुपयों के विषय में बहुत सावधान रहे । तत्पश्चात् वह शान्तिपूर्वक उपरिपुल को पार कर अपने डिब्बे में प्रवेश किये तथा थोड़ा दिव्य नाम का कीर्तन किया। गाड़ी तभी चली। इस प्रसंग में स्वामी जी के मन की अनुद्विग्न अवस्था तथा उनकी करुणा को सुन्दरतापूर्वक स्पष्ट किया गया है जो वैयक्तिक कठिनाई के सभी विचारों पर अभिभावी हो जाती हैं।
स्वामी जी केवल भगवान् को जानते हैं तथा उनकी इच्छाओं को कार्यान्वित करने के लिए जीवन-यापन करते हैं। वह भविष्य के लिए योजना नहीं बनाते हैं। वह प्रत्यासन्न कार्य में अपनी समग्र सत्ता लगा देते हैं। उनके लिए सभी कार्य समान महत्त्व के हैं। एक बार वह जर्मनी के कोल्न में सत्संग में थे। सत्संग के अन्त में लोग भावप्रवणता से उनके चारों ओर एकत्र हो गये। स्वामी जी को कुछ ही समय में विमान पकड़ना था। किन्तु आयोजक जब बड़ी ही उत्सुकता से अपनी घड़ियों की ओर देख रहे थे और सन्देह कर रहे थे कि स्वामी जी वायुयान पकड़ भी सकेंगे, उस समय वह भक्तों के भावों का विनिमय करते हुए शान्तिपूर्वक बैठे थे तथा उनसे बातें कर रहे थे। बहुत देर के पश्चात् जब स्वामी जी उठ ही रहे थे कि एक महिला अकस्मात् अन्दर आयी और अपनी मरणासन्न माँ को, जिसे वह वहाँ अपने साथ लायी थी, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए थोड़ा समय देने के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी तुरन्त ही उस वृद्ध महिला के पास गये और उसके बहुत निकट घुटने टेक कर बैठ गये तथा भगवान् से उसकी शान्ति के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी जब हार्दिक प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने आनन्दभाव की अनुभूति की। यह कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् ही उन्होंने स्विट्जरलैण्ड के लिए वायुयान पकड़ने के लिए उस स्थान से प्रस्थान किया। निस्सन्देह, आयोजकों को अब तक पक्का विश्वास हो गया था कि वायुयान प्रस्थान कर गया होगा। किन्तु ऐसा हुआ कि वायुयान विलम्ब से आया और स्वामी जी को उससे वंचित नहीं रहना पड़ा। भले ही उनका वायुयान छूट जाय-यद्यपि अपने सेवा-कार्य के लिए अनेक बार ऐन मौके पर उनके रुक जाने के बावजूद ऐसा कभी नहीं हुआ-किन्तु कुछ भी हो, यह कभी उनकी चिन्ता का विषय नहीं बना । अन्तिम क्षण में भी कोई उतावली नहीं थी। अन्तिम पल तक प्रत्येक विषय पर यथावश्यक ध्यान दिया और तभी वह कार्यक्रम के अनुसार स्विट्ज़रलैण्ड में भगवत्कार्य सम्पन्न करने को स्वतन्त्र हुए।
एक बार स्वामी जी रेलगाड़ी द्वारा उत्तरी भारत की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने पहले की तरह ही प्लेटफार्म पर लोककल्याणार्थ प्रार्थना करते हुए कीर्तन किया और जब गाड़ी चलने लगी तो वह अपने डिब्बे में चले गये। उस समय तक कोई धनाढ्य व्यवसायी अन्दर आ गया था और स्वामी जी का बिस्तर फेंक कर उनको आवण्टित शायिका पर निश्चिन्त बैठा था। उन्होंने उसे अपने साथ चल रहे भक्त प्रातःस्मरणीय रामरतन जी से व्यंग्यपूर्वक यह कहते हुए सुना कि किसी ने स्वामी जी को प्रथम श्रेणी का किराया दान में दे दिया होगा। क्रुद्ध रामरतन जी उसे मुँहतोड़ जवाब देने ही वाले थे कि स्वामी जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि सेठ जी ने ठीक ही कहा था। संन्यासी होने से उन्हें गद्दों का सुख नहीं उठाना चाहिए। ऐसा कह कर, उन्होंने शायिका के पार्श्व में फ़र्श पर अपना बिस्तर बिछा दिया और उस पर लेट गये। स्वामी जी ने जिस अक्षुब्ध तथा तुष्ट ढंग से शायिका पर अपने अधिकार को विनम्रतापूर्वक जाने दिया उसने सेठ जी के ऊपर तत्काल प्रभाव डाला तथा उसे पता चल गया कि वह एक असाधारण व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा है। उसने स्वामी जी से पश्चात्तापपूर्वक क्षमा-याचना की और अपनी शायिका पर वापस आने के लिए उनसे प्रार्थना की। ऐसी स्थिति में अल्पतर मानसिक सन्तुलन तथा विनम्रता वाला कोई भी व्यक्ति प्रतिवाद करता तथा वहाँ तमाशा खड़ा कर देता। स्वामी चिदानन्द, जो पूर्ण अनात्मशंसा की स्थिति से गुजर चुके थे, नहीं समझते थे कि यह अप्रसन्न तथा उत्तेजित होने का कोई अवसर है। यहाँ पुनः एक अनुकरणीय चेष्टा थी। जब उन्होंने देखा कि सेठ जी सच्चे अनुताप से भरे हुए हैं तो बह हठपूर्वक फर्श पर पड़े रहने के बजाय बिना किसी बतंगड़ के शान्तिपूर्वक शाविका पर चले गये। भगवान् गीता में कहते हैं: "जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सन्तप्त नहीं होता और जो स्वयं अन्य किसी व्यक्ति से सन्ताप नहीं प्राप्त करता एवं जो हर्ष, अमर्ष, भय तथा उद्वेग से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है।... वह शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में सम है।... वह निन्दा तथा प्रशंसा को तुल्य समझने वाला, मौनव्रतावलम्बी, बत्किंचित् प्राप्त होने पर सन्तुष्ट रहने वाला तथा आश्रय-रहित होता है...।" समचित्तता के इस शास्त्रीय चित्रण को सम्यक् रूप से समझने के लिए उसे स्वामी जी में देखने की आवश्यकता है।
स्वामी जी, जैसा कि पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, कभी कोई सिद्धि प्रदर्शित नहीं करते हैं; किन्तु किन्हीं अत्यावश्यक अवसरों पर उनके रोगहर स्पर्श तथा सरल प्रार्थना ने वास्तव में चमत्कारिक परिणाम दिखलाया है। बहुत ही करुणार्द्र तथा कोमल हृदय होने के कारण वह पीड़ित लोगों को देख कर द्रवित हो उठते हैं तथा ऐसे अनेक अवसरों पर उनकी प्रार्थनाएँ तात्क्षणिक आभिचारिक स्वस्थता लाती हुई देखी गयी हैं। एक बार सन् १९५३ में ग्रीष्म ऋतु की अन्धकारपूर्ण रात्रि में जब वह दिल्ली के एक भक्त श्री इन्द्रजीत शर्मा से बातें कर रहे थे, उन्हें सहसा एक चीख सुनायी पड़ी। एक अल्पवयस्क बालिका को एक विषैले बिच्छू ने डंक मार दिया था। स्वामी जी तत्काल उसे कुटीर में ले गये तथा उसे बेंच पर लेट जाने को कहा। वह एक तौलिया ले आये तथा उसके प्रभावित अंग पर उसे रगड़ते रहे और इसके साथ ही भगवन्नाम का उच्चारण भी करते रहे। उन्होंने न तो किसी औषधि अथवा जड़ीबूटी का प्रयोग किया और न विहित मन्त्रों में से किसी एक का उच्चारण ही किया। तथापि वह बालिका शीघ्र ही पीड़ामुक्त हो गयी। वह प्रसन्नतापूर्वक यह कहते हुए कि अब उसे कोई पीड़ा नहीं हो रही है, पूर्ण स्वस्थ चित्त से तत्काल उठ खड़ी हुई।
राउरकेला के आध्यात्मिक सम्मेलन में स्वामी जी एक बार लोगों से व्यक्तिगत वार्ता के लिए मंच से कुछ समय के लिए चले गये। उड़ीसा के भूतपूर्व मन्त्री श्री मदनमोहन प्रधान भी, जिन्हें उस समय तीव्र ज्वर था, स्वामी जी का दर्शन करने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आये थे। उनके साथ के एक भक्त ने स्वामी जी को बताया कि श्री प्रधान को तीव्र ज्वर है। इस पर स्वामी जी ने उनको करुणापूर्ण दृष्टि से देखा, उनके हाथ को पकड़ लिया और कहा - "आपको ज्वर नहीं है।" किसी तरह ज्वर अदृश्य हो गया तथा श्री प्रधान अपने को तत्काल पूर्ण स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट पा कर आश्चर्यचकित रह गये।
भंजनगर के एक वृद्ध भक्त श्री राजू सुबुद्धि ने स्वामी जी की रोगनिवारण की चमत्कारिक शक्ति का वर्णन इस लेखक से किया है। एक बार जब स्वामी जी साधना-शिविर के सम्बन्ध में भंजनगर में थे तब यह सज्जन उनसे मिले तथा उन्हें कई महीनों से अपने प्रमस्तिष्कीय भाग में असहनीय जलन से उत्पन्न घोर यन्त्रणा का विवरण दिया। स्वामी जी ने कृपापूर्वक उन भक्त के शिर पर मात्र अपना हाथ रखा मानो कि वह जलन की तीव्रता का पता लगा रहे हों। और, उतना ही पर्याप्त था। अकस्मात् वृद्ध सज्जन ने अपने शिर में एक हिम-शीत विद्युत्-धारा-सी दौड़ती हुई अनुभव की और वह सदा के लिए पीड़ा-मुक्त हो गये।
स्वयं इस लेखक को भी सम्बलपुर में, जहाँ उसे सत्ताईसवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन के महासचिव का कार्य करने का संयोग हुआ, स्वामी जी के आशीर्वाद की शक्ति का एक अविस्मरणीय अनुभव हुआ। उसे सम्मेलन के दूसरे दिन एक तार प्राप्त हुआ कि उसके पिता को सुदूर गंजाम जिले के अपने ग्राम में अंगघात हो गया है और वह संकटपूर्ण स्थिति में पड़े हुए हैं। तार प्राप्त होने पर उसे चिन्ता तथा व्यथा हुई। स्वयं कुछ निर्णय न कर सकने के कारण उसने उस तार के कागज के शीर्ष पर यह अंकित कर कि 'कृपया इस सेवक को वर्तमान स्थिति में उसके कर्तव्यों के विषय में आदेश दें' स्वामी जी के पास अग्रसारित कर दिया। जब कागज स्वामी जी के पास पहुँचाया गया तो वह कुछ लिखने में तल्लीन थे। तथापि, जब मौखिक रूप से सन्देश पहुँचाया गया तब वह एक क्षण रुके तथा शिर उठाये बिना ही उन्होंने उच्च स्वर से कहा- "कोई अमंगल नहीं होगा। यह समय नहीं है। संकट का निवारण हो गया है।" तत्पश्चात् उन्होंने विचारपूर्वक आगे कहा- "हाँ, यदि बेहेरा जी चाहें तो वह निश्चय ही जा सकते हैं।" स्वामी जी के शब्दों से बल प्राप्त कर इस सेवक ने रुके रहना ही पसन्द किया; क्योंकि सम्मेलन दो दिन और चलने वाला था। अगले दिन ही उसे यह समाचार-सूचक तार मिला कि उसके पिता की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। इस सेवक के हृदय में करुणाशील गुरुदेव के प्रति जो गम्भीर कृतज्ञता का भाव उमड़ आया उसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। उसके पूर्वगामी दिवस को पूज्यचरण स्वामी जी ने सम्मेलन में उपस्थित लगभग दश सहस्र भक्तों के समुदाय से रोगी के प्रकृतिस्थ होने के लिए अपने साथ महामृत्युंजय मन्त्र का दश बार जप करने का अनुरोध किया था। स्वामी जी की इच्छा ने वैश्व-इच्छा से एकाकार हो कर दूर-उपचार का कार्य किया तथा रोगग्रस्त पिता की आसन्न मृत्यु से रक्षा की। इस सेवक ने बाद में जब एकत्रित जिज्ञासुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया तथा मन्त्र की आभिचारिक प्रभावोत्पादकता के विषय में सूचित किया तो उन्होंने भी महामृत्युंजय मन्त्र के प्रभाव को अनुभव किया। उस संकटकालीन अवसर पर स्वामी जी ने जैसा पूर्ण प्रशान्ति के साथ आश्वासन दिया वैसा आश्वासन कोई विरल दिव्य व्यक्ति ही दे सकता है।
सिद्ध योगी में अपरिमेय शक्ति होती है। (पंच) भूतों पर उसका प्रभुत्व होता है। किन्तु वह सदा ही प्रेम तथा समर्पण के मार्ग पर चलता है। वह केवल भगवदिच्छा की पूर्ति चाहता है। तथापि ऐसे अवसर भी आते हैं जब वह विपद्मस्त लोगों की रक्षा करने के लिए दैवी अन्तः प्रेरणा से प्रभावित हो जाता है। इसी तरह ऐसे अवसर आये हैं जब स्वामी जी (पंच) भूतों में हस्तक्षेप-सा करते प्रतीत हुए। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन-काल में एक ऐसा ही प्रसंग आया। बेगम पेठ में स्वामी जी का विश्राम-स्थल सभा-स्थल से लगभग पाँच मील की दूरी पर था। सम्मेलन के दूसरे दिन जब वह अपने विश्राम स्थल से प्रस्थान करने वाले थे कि असामान्य रूप से मूसलाधार वर्षा हुई। स्वामी जी ने अपने साथ के भक्तों से यों ही पूछा कि क्या उस समय हैदराबाद में वर्षा की अपरिहार्य आवश्यकता है। भक्तों ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया। तब स्वामी जी मौन हो गये तथा वर्षा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच सम्मेलन-स्थल पर एकत्रित प्रतिनिधि काले बादलों को देख कर खिन्न हो रहे थे; क्योंकि सम्मेलन का आयोजन एक खुले मैदान में किये जाने के कारण अल्पकालिक वृष्टि भी उसे पूर्णतः अस्तव्यस्त कर डालती। वे बादल जो कुछ ही क्षण पूर्व सभी दिशाओं से घिरते आ रहे थे, किसी तरह, बिना वृष्टि किये ही प्रस्थान कर गये जिससे सभी को परम आश्चर्य तथा निश्चिन्तता हुई। जब स्वामी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने नगर के दूसरे भाग में हुई घोर वृष्टि के कारण अपने विलम्ब से पहुँचने के लिए क्षमा-याचना की। उन्होंने वर्षा से सभा-स्थल की रक्षा करने के लिए भगवान् तथा गुरुदेव को धन्यवाद दिया। कई लोगों के लिए यह किसी चीज़ की विशेष द्योतक नहीं लग सकती; किन्तु भक्तों तथा सम्मेलन के आयोजकों को कोई सन्देह नहीं रहा कि यह पंचभूतों पर स्वामी जी के प्रभाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी।
इसी भाँति बेंगुलूरु में आयोजित छब्बीसवें अखिल भारत दिव्य जीवन सम्मेलन के अवसर पर वहाँ पूर्व-रात्रिभर भीषण वर्षा होती रही। सम्मेलन के दिन प्रातःकाल हो जाने पर भी वर्षा हो रही थी तथा मौसम अनिष्टसूचक था। आयोजकों ने सम्मेलन स्थगित करने का विचार किया। इस पर एक सुप्रसिद्ध भक्त रामरतन ने दृढतापूर्वक कहा, "आपको मालूम होना चाहिए कि पंच महाभूतों पर स्वामी जी का प्रभुत्व है। आपको स्वामी जी में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए तथा उनके हस्तक्षेप करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए।" भक्तों ने प्रार्थना की। और सम्मेलन से ठीक कुछ घण्टे पूर्व निश्चित रूप से बादल पूर्णतया छँट गये। दिन धूपमय था तथा अत्युष्ण सूर्य ने पंकिल भूमि को तत्काल शुष्क बना दिया। जो लोग वहाँ उद्घाटन के समय पहुँचे वे यह विश्वास नहीं कर सके कि कुछ घण्टों पूर्व वहाँ की स्थिति इतनी निराशाजनक थी। स्वामी जी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करते, किन्तु मात्र उनकी उपस्थिति तथा सरल प्रार्थनाओं से रहस्यमय ढंग से चमत्कार होते हैं। और जब वे घटित होते हैं तो वह शिशुवत् सरल भाव से अन्य लोगों के साथ खड़े हो कर चमत्कारों की क्रिया को ऐसे देखते हैं मानो कि वे भगवान् तथा गुरुदेव की कृपा से हो रहे हों।
स्वामी जी अपने दिव्य स्वरूप में नित्य निवास करते हैं तथा सम्पूर्ण विश्व को उसी तत्त्व से आवृत देखते हैं। उनका जीवन इस सत्य पर आधारित है कि यह समस्त जगत् ईश्वर से व्याप्त है। अपने प्रत्येक कर्म द्वारा वह मानव जाति को यह शिक्षा देते हैं कि यह संसार भगवान् का ही प्रकटीकरण है तथा दिव्य तत्त्व से ओतप्रोत है। यही वह रहस्य है जिसे वह अपने आचरण तथा उपदेश द्वारा प्रकट करते हैं।
एक बार श्री दुर्लभचन्द्र चौधरी के नेतृत्व में उड़ीसा के कुछ भक्त स्वामी जी का दर्शन करने रायगढ़ गये। जब वे स्वामी जी के शिविर में पहुँचे तो उन्होंने ठीक उसी समय स्वामी जी को कार से उतरते हुए देखा। साष्टांग प्रणाम के पश्चात् दुर्लभ जी ने पूछा, "स्वामी जी का स्वास्थ्य कैसा है?" इसके उत्तर में स्वामी जी ने आनन्दपूर्वक अपना प्रिय वेदान्त-गीत गाया : "हर हाल में अलमस्त सच्चिदानन्द हूँ- मैं प्रत्येक परिस्थिति में सत्-चित्-आनन्द हूँ।" उस समय के उनके उस सहज, गम्भीर दृढ़ कथन ने भक्तों के हृदय पर अपनी गम्भीर छाप छोड़ी। तथापि उन्होंने तत्काल ही आगे कहा, "भगवान् ने जैसे रखा है।" अर्थात् भगवान् का जैसा विधान है। स्वामी जी ने उसी नगर में एक दिन सायंकाल को स्थानीय विधिज्ञ-परिषद् में भाषण दिया। भाषण के अन्त में वहाँ उपस्थित विशिष्ट लोगों से उनका परिचय कराया गया। जब स्वामी जी की बारी आयी तो उन्होंने अपने साथ आये हुए भक्तों का परिचय कराना आरम्भ कर दिया ऐसा करते समय उन्होंने दिव्य जीवन संघ की रायगढ़ शाखा के सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा का उल्लेख अपने गुरुभाई के रूप में किया। एक युवक विधिज्ञ ने ध्यान दिलाया कि इससे पूर्व डा. शर्मा ने स्वामी जी का उल्लेख गुरुदेव के रूप में किया था और उसने जानना चाहा कि क्या इन दोनों कथनों में कुछ विरोध है। स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि गुरुदेव शिवानन्द जी महाराज ही शर्मा जी के गुरु थे; किन्तु शर्मा जी उनसे दीक्षा नहीं ग्रहण कर सके थे, अतः गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने शर्मा जी को दीक्षा दी। विधिज्ञ इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ और वाद-विवाद जारी रखना चाहता था, किन्तु तब स्वामी जी तत्काल सहसा गम्भीर हो गये और आगे कहा, "मेरे लिए तो वह साक्षात् नारायण हैं।" वह चाहते थे कि सभी लोग नारायण-सूक्त में वर्णित सभी पदार्थों के चरम स्वरूप का अनुभव करें। वह इस वैदिक पाठ से प्राय: यह सूक्त उद्धृत करते हैं :
"यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।
अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥"
इस सम्पूर्ण जगत् के अन्दर तथा बाहर जो कुछ भी सुनायी अथवा दिखाया पड़ता है, वह सब नारायण से व्याप्त है। यही उनके जीवन-गीत का प्रमुख भाव है। वह प्रत्येक रूप में भगवान् का दर्शन करते हैं। एक बार एक भक्त अपने परिवार के साथ आश्रम आया तथा स्वामी जी से श्री गुरुदेव के समाधि मन्दिर में अपने बच्चे का अन्नप्राशन-संस्कार कराने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने इस विधि को जिस प्रकार सम्पन्न किया उसने उसे स्मरणीय बना डाला। उन्होंने सम्पूर्ण क्रिया को आध्यात्मिक बना दिया। प्रथम वह उस बच्चे के सम्मुख ऐसे बैठे जैसे कि उत्कट भक्त गोपालकृष्ण के सामने बैठता है। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से बालकृष्ण की प्रार्थना की तथा पूर्ण हार्दिकता तथा प्रेम के साथ बच्चे को अपनी गोद में आने के लिए आमन्त्रित किया, उससे प्रार्थना भी की। तत्पश्चात् उन्होंने बड़े ही स्निग्ध तथा मृदु ढंग से उसे मधुर पायस खिलाया। उन्होंने थाली का शेष पायस इस लेखक-सहित वहाँ एकत्रित सभी लोगों को प्रसाद के रूप में दिया और उसमें से थोड़ा-सा स्वयं भी खाया। उनके लिए वह बच्चा मानव-शिशु मात्र न था, अपितु दिव्यता का शुद्ध प्रकटीकरण था।

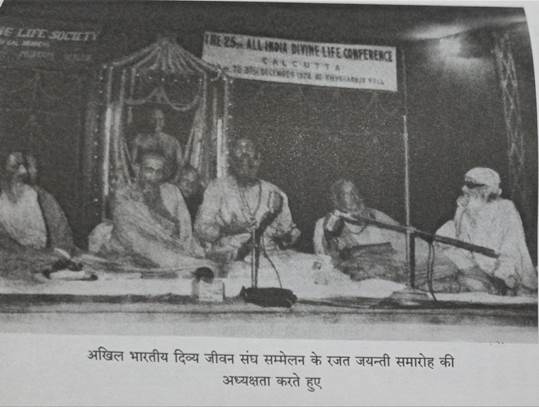


एक अन्य अवसर पर जब स्वामी जी उड़ीसा के गंजाम जिले में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने बालीपदार से बुगुडा के मार्ग में छोटे-छोटे बालकों की एक टोली को राजपथ के किनारे खेलते हुए देखा। उन्होंने चालक को गाड़ी रोकने के लिए कहा और उनमें बाँटने के लिए केलों का एक गुच्छा निकाला और इस कार्य को करने को दुर्लभ जी को कहा। दुर्लभ जी गाड़ी से उतरे तथा बालकों को जोर से पुकारा कि वे पास आ कर केले ले जायें। इस पर बालक यह समझ कर कि यह कोई जाल है, भाग गये। स्वामी जी ने दुर्लभ जी को उनके अविनीत व्यवहार के लिए हलकी-सी फटकार दी तथा उन्हें समझाया, "बालक हमसे किसी पदार्थ की आशा नहीं रखते। अतः उन्हें यहाँ बुलाने के स्थान में आपको भावपूर्वक उनके पास जा कर उन्हें प्रेमपूर्वक खिलाना चाहिए।" दुर्लभ जी ने तदनुसार ही कार्य किया तथा स्वामी जी के आदेश के आध्यात्मिक भाव को पूर्ण रूप से समझ कर उन्होंने कहा- "स्वामी जी! अब मैंने समझा, इसका उद्देश्य एक पूजा था।" इस पर स्वामी जी ने आगे कहा, "हाँ, महापूजा।" केवल शारीरिक कर्म ही नहीं अपितु विचार प्रक्रिया का आध्यात्मीकरण ही भोजन कराने को सरल बालकों के रूप में प्रकट भगवान् को अर्पित भेंट में रूपान्तरित करता है।
स्वामी जी को सम्बलपुर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित 'ज्योति विहार' के अपने आवास-काल में एक बार अपने शिर का मुण्डन कराने के लिए एक नापित की आवश्यकता पड़ी। जब नापित आया तो स्वामी जी ने सौजन्यतापूर्वक उससे उसका नाम पूछा। नापित ने बतलाया कि उसका नाम माधव है। इस पर स्वामी जी ने नापित के रूप में उनकी सेवा करने वाले माधव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया जिससे वह परम आश्चर्य में पड़ गया। नापित की सेवाएँ प्राप्त करने के पूर्व उन्होंने सर्वप्रथम उस व्यक्ति को अपनी हार्दिक प्रार्थना निवेदित की। क्षौर-कर्म समाप्त होने पर स्वामी जी ने उसे भोग के रूप में प्रचुर फल तथा दक्षिणा के रूप में कुछ सिक्के दिये। इस भाँति वह अपने वैयक्तिक उदाहरण द्वारा यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि जिज्ञासु को मानव में माधव का दर्शन करना चाहिए तथा मनुष्यत्व से देवत्व में उन्नत होना चाहिए।
ऐसी असंख्य घटनाएँ होंगी, स्वामी जी के दिव्य व्यक्तित्व के सुरभित सत्त्व को अभिव्यक्त करने वाले अगण्य पुष्प होंगे। उनका जीवन यह तथ्य व्यक्त करता है कि भगवान् अन्तरिक्ष के कण-कण में व्याप्त हैं। रहस्यवादी तुलसीदास की भाँति ही वह सर्वत्र तथा सबमें भगवती सीता माता तथा भगवान् रामचन्द्र के दर्शन करते हैं। ऐसा सन्त जो सर्वत्र भगवान् को देखता है तथा भगवान् के अन्दर समस्त विश्व को देखता है, नित्य ईश्वरीय चेतना में स्थित रहता है। वह निस्सन्देह एक विरल दिव्य व्यक्ति है जो अनेक जन्मों की दीर्घकालिक साधना के अनन्तर यह अनुभव कर लेता है कि यहाँ जो-कुछ भी है, वह सब भगवान् से व्याप्त है। भगवान् गीता में कहते हैं: "ज्ञानवान् व्यक्ति बहुत जन्मों के अतिक्रमण के पश्चात् समस्त जगत् वासुदेव-रूप है, इस प्रकार मुझे प्राप्त करता है, सुतरां ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है" (७/१९)।
उनके इस अहंभाव के परम राहित्य तथा दृष्टि की निर्दोष शुचिता के कारण गुरुदेव ने दृढ़तापूर्वक कहा था, "यह उनका अन्तिम जन्म है।" चिदानन्द निस्सन्देह वह प्रबुद्ध सन्त हैं, विरल दिव्य व्यक्ति हैं जो अनेक जन्मों की तपस्या के सुकृत के परिणामस्वरूप आज सर्वत्र भगवान् को देखते हैं और उनमें ही सदा-सर्वदा स्थित हैं। भगवत्साक्षात्कार-प्राप्त आत्माओं में वह मानव जाति के वरदान के रूप में विभासित हैं। अब यह मनुष्य के हित में है कि वह उनका आह्वान सुने, "हे मानव! तुम दिव्य हो। तुम यह भौतिक शरीर नहीं हो, तुम यह चंचल मन भी नहीं हो। तुम ज्योतिर्मय दिव्य आत्मा हो। तुममें से प्रत्येक व्यक्ति दिव्य व्यक्ति है।" वह मनुष्य के पास मसीहा के रूप में आये हैं और इस महान् पाठ की शिक्षा देने के लिए एक घर से दूसरे घर, पूर्व से पश्चिम तथा तुच्छ छोटी झोपड़ी से भव्य भवन के लोगों में विचरण कर रहे हैं कि मनुष्य पाशविकता त्याग दे और मनुष्यता से देवत्व तक उन्नत बने और इस भाँति मानव-जीवन के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करे।
एकादश अध्याय
शिक्षा का भण्डार
"ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते
-कोई-कोई महात्मा ज्ञान-रूप यज्ञ द्वारा मेरी आराधना करते हैं" (गीता : ९/१५) ।
"मुझे उनकी प्रतिभा का पता चल गया है।... वह अब मुझसे बच कर निकल नहीं सकते।" गुरुदेव ने अपने मिलन के प्रारम्भिक काल में ही एक दिन अपने महत्तम शिष्य के विषय dot 4 इस प्रकार हर्षपूर्वक घोषणा की थी। तबसे हिमालय की निर्जन कन्दराओं में अपनी गम्भीर साधना तथा अज्ञात संचरण के अतिरिक्त ऐसा कदाचित् ही कोई दिन व्यतीय हुआ हो जब स्वामी जी ने कोई प्रेरणादायी भाषण न दिया हो या कोई ज्ञानगर्भित अप्रतिम लेख न लिखा हो। इन पाण्डित्यपूर्ण लेखों में विशाल क्षेत्र की शैलियों तथा विषयों का समावेश किया गया है। इनकी रचना पर्याप्त वैविध्यपूर्ण अवसरों पर की गयी है तथा ये विविध व्यवसाय तथा भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले आधुनिक मानव की समझ तथा उपयोग के उपयुक्त सर्वाधिक व्यापक आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।
वह जिस वर्ष गुरुदेव के पास गये, उसी वर्ष उन्होंने अद्भुत निपुणता तथा उत्साह से गुरुदेव की अमर तथा अद्वितीय जीवनी 'लाइटू फाउण्टेन' (Light Fountain- 'आलोक-पुंज') की रचना की। गुरुदेव के जीवन की इस आध्यात्मिक व्याख्या में उन्होंने उनके जीवन तथा उपदेशों के गहनतर पक्षों को ऐसा अनावृत किया जैसा कि इससे पूर्व अन्य किसी ने नहीं किया था। यह ग्रन्थ अपनी प्रबल भावप्रवणता से स्वयं गुरुदेव का प्रशंसास्पद बना। यह जीवनी गुरुदेव के आत्मविकास, आन्तर प्रस्फुटन तथा आध्यात्मिक पूर्णता का सुगम्भीर रहस्योद्घाटन करने वाला प्रलेख है। स्वामी जी ने इसमें एक महान् आध्यात्मिक जीवन के गुह्य तथा वैयक्तिक साधना के अतिरिक्त सामान्य मानवीय संवेदनाओं से सम्बन्धित छोटी-छोटी चीजों के महत्त्व को प्रकट किया है। उन्होंने दर्शाया है कि गुरुदेव ने किस प्रकार अपनी साधना प्रतीयमानतः तुच्छ विषयों से आरम्भ की थी। वह गुरुदेव की दैनन्दिनी से निम्नांकित स्वगृहीत अनुशासनों को उद्धृत करते हैं: "नमक का सेवन छोड़ दो। चीनी का सेवन छोड़ दो। मसाले का सेवन छोड़ दो। सब्जी का सेवन छोड़ दो। मिर्च का सेवन छोड़ दो। इमली का सेवन छोड़ दो। यदि आप इन सब बातों का अभ्यास नहीं करते तो आप सच्चे साधु नहीं बन सकेंगे।" यह गुरुदेव की विस्मयकारी सहिष्णुता का रहस्य है जिसने उन्हें इतना महान् बनाया। वह चाहते थे कि उनके शिष्य यह जान लें कि साधना को ध्यान कक्ष तक ही सीमित नहीं रखना है, सभी कार्यों को पूजा में रूपान्तरित करना है तथा सम्पूर्ण व्यक्तित्व का दिव्यीकरण करना है। स्वामी जी ने इस आध्यात्मिक रहस्य को लाइट् फाउण्टेन में एक बहुत ही स्मरणीय शैली में प्रकट किया है। उन्होंने दर्शाया है कि आध्यात्मिक सत्य किस प्रकार शास्त्रों के पृष्ठों के पुष्पित पदसमूह न हो कर गुरुदेव जैसे सन्तों के जीवन के भावात्मक तथा व्यवहारात्मक तथ्य हैं।
महत्त्व की दृष्टि से इस प्रकाशप्रद जीवनवृत्तात्मक निबन्ध के पश्चात् स्वामी जी की देवी-माहात्म्य की अमूल्य व्याख्या आती है। उन्होंने १९५३ के शरत्काल में आश्रम में भगवती माँ के नवरात्र-पूजाकाल में नौ भाषण दिये जो गुणात्मक दृष्टि से गम्भीर तथा गीतात्मक थे। उन्होंने श्रोताओं को अपनी शैली में जो गम्भीर होने के साथ-ही-साथ सूक्ष्म भी थी मानव-मन में गहराई से निविष्ट आसुरी शक्तियों के स्वरूप को हृदयंगम कराया। महाकाली के रूप में भगवती माँ साधक को इन विनाशकारी शक्तियों को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करती हैं। स्वामी जी ने विनाश की हितकारी प्रक्रिया को प्रतिजैविकी (एन्टिबाइआटिक) के एक सुसंगत आधुनिक उदाहरण से स्पष्ट किया। ये औषधियाँ प्रबल जीवाणु-नाशक हैं, किन्तु जीवन-रक्षक भी हैं। विनाश वह काष्ठफलक है जिस पर सृजन कार्य आरम्भ होता है। स्वामी जी ने महाकाली के रूप में माँ की प्रथम तीन दिन की पूजा का उपसंहार करते हुए लोगों से अपने अन्दर के पशु की बलि देने का अनुरोध किया। आसुरी शक्तियों की पकड़ से एक बार छुटकारा पा लेने पर वह माँ की महालक्ष्मी के रूप में पूजा करने का अधिकारी बन जाता है। यह (महालक्ष्मी) माँ का वह रूप है जिसमें उनकी परवर्ती तीन दिनों में पूजा की जाती है जो व्यक्ति को अष्ट ऐश्वर्यों से सम्पन्न बनाती है। किन्तु सद्भक्त केवल दैवी सम्पत् की ही अभिलाषा करते हैं। दैवी सम्पत् से सम्पन्न हो कर साधक अन्ततः महासरस्वती की पूजा करने योग्य बन जाता है। स्वामी जी ने बल दिया कि मितभाषण, सत्यभाषण तथा मधुरभाषण महासरस्वती की व्यावहारिक पूजा है। गुह्य अर्थों में महासरस्वती गुरु-प्रदत्त पवित्र मन्त्र का साकार रूप भी है। गुरु-मन्त्र का जप महासरस्वती की सर्वोत्कृष्ट कोटि की पूजा है। यह पूजा अन्त में साधक को परम ज्ञान से सम्पन्न बनाती है। स्वामी जी ने दर्शाया है कि किस प्रकार ऐसी प्रक्रिया द्वारा दशम दिवस को महिमामय विजय-दिवस के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी द्वारा इस प्रकार सुन्दर रूप से प्रतिपादित नवरात्र-पूजा के अन्तरंग आध्यात्मिक तात्पर्य को बाद में 'गाड ऐज मदर' (God as Mother- 'भगवान् का मातृरूप') के नाम से प्रकाशित किया गया।
स्वामी जी बहुत पूर्व सन् १९४६ में कौशिक कृतकनाम से गुरुदेव के विषय में अनेक लेख लिखा करते थे। उन लेखों में गुरुदेव के दिव्य व्यक्तित्व का गम्भीर ज्ञान व्यक्त किया गया है। गुरुदेव के ७० वें जन्मदिवसोत्सव (Platinum Jubilee) के अवसर पर सन् १९५७ में उन लेखों को संकलित कर 'वर्ल्ड गाइड शिवानन्द' (World Guide Sivananda) शीर्षक से प्रकाशित किया गया। अपनी विशद ज्ञानग्राह्यता के लिए विश्रुत यह ग्रन्थ प्रत्येक साधक के लिए एक अमूल्य सहायक है।
स्वामी जी विविध लोकप्रिय उपायों से गुरुदेव के सन्देश का प्रचार करने को उत्सुक थे। उदाहरणार्थ कौतुकागारशास्त्र लोगों को रोचक ठोस ढंग से प्रशिक्षित बनाने का प्रयास करता है, अतः स्वामी जी ने इस प्रविधि को आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए काम में लिया तथा योग-कौतुकागार की स्थापना की। उन्होंने गुरुदेव द्वारा उपयोग की हुई सामग्री तथा उनकी प्रारम्भिक काल की तपश्चर्या के स्थानों के चित्रात्मक प्रतिरूपों को एकत्र कर उन्हें सँजोया। उन्होंने सन् १९५८ में योग-कौतुकागार की सन्दर्शिका के रूप में 'शिवानन्द रिगेलिया' (Sivananda Regalia) पुस्तक की रचना की। बारह अध्यायों में विभाजित इस लघु पुस्तक में केवल चौरासी मुद्रित पृष्ठ हैं; किन्तु इसका विषय, जो कि गुरुदेव के चरणों में पुष्पार्पण-रूप है, प्रत्येक पाठक के लिए एक रोमांचकारी अपूर्व आध्यात्मिक अनुभव का रूप प्रदान करता है। इसमें स्वर्गाश्रम का कुटीर १११ जिसमें गुरुदेव ने अठारह वर्षों तक घोर तप किया था अथवा अन्नक्षेत्र जिसे उन्होंने आश्रमवासियों तथा अभ्यागतों की अतिथि-सेवा के लिए स्थापित किया था का वर्णन ऐतिहासिक स्थानों के रूप में न कर गुरुदेव के दिव्यीकरण की साधना की एक विषयपरक आधारशिला के रूप में किया गया है।
स्वामी जी सदा ही नवयुवक छात्रों का विशेष लिहाज रखते हैं। एक विशेष भेटवार्ता में, जो उन्होंने १९५९ में एक छात्र-मण्डली से की लिपिबद्ध तथा 'स्ट्यूडेन्ट्स, स्पिरिट्यूअल, लिटरेचर ऐण्ड शिवानन्द' (Students, Spiritual Literature and Sivananda - 'छात्र, आध्यात्मिक साहित्य तथा शिवानन्द) के नाम से एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की गयी है। उसमें वह उन्हें भारतीय संस्कृति के देदीप्यमान प्रकाश-स्तम्भ बनने को प्रोत्साहित करते हैं। वह उन्हें गुरुदेव के 'ऐड्वाइस टु स्ट्यूडेन्ट्स' (Advice to Students - 'छात्रों को उपदेश'), 'प्रैक्टिस आव् ब्रह्मचर्य' (Practice of Brahmacharya - 'ब्रह्मचर्य-साधना'), 'शुअर वेज़ आव् सक्सेस इन लाइफ़ ऐण्ड गॉड् रिअलाइजेशन' (Sure Ways of Success in Life and God-realisation-'जीवन में सफलता के रहस्य तथा भगवत्- साक्षात्कार'), 'एथिकल टीचिंग्स' (Ethical Teachings - 'नैतिक शिक्षा'), 'स्ट्यूडेन्ट्स सक्सेस इन लाइफ' (Students' Success in Life - 'विद्यार्थी जीवन में सफलता') तथा 'डिवाइन लाइफ फार चिल्ड्रेन' (Divine Life for Children -'बालकों के लिए दिव्य जीवन-सन्देश' जैसी पुस्तकों के अध्ययन तथा नैतिक अनुशासन के दृढ़ आधार पर अपने जीवन का निर्माण करने का परामर्श देते हैं। वह आग्रह करते हैं कि जीवन-रूपी वृक्ष को प्रतिदिन स्वाध्याय-रूपी वृष्टि से सींचने की आवश्यकता है। वह उनके सम्मुख आहार, विचार तथा व्यवहार की कुछ बहुत ही विवेकपूर्ण आदतों से निर्मित एकमुश्त कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तथा सूचित करते हैं कि इससे उनकी भौतिक उन्नति तथा आध्यात्मिक सफलता दोनों ही सुनिश्चित रहेंगी।
जब १९४८ में गुरुदेव ने योग-वेदान्त-आरण्य-विश्वविद्यालय (अब विद्यापीठ) की स्थापना की तो स्वामी जी इस संस्था के कुलपति तथा राजयोग के प्राध्यापक के रूप में इसके प्राण थे। उन्होंने लगभग एक दशक तक कक्षाएँ चलार्थी तथा श्रृंखलाबद्ध अत्यन्त शिक्षाप्रद तथा प्रेरक भाषण दिये जिन्हें १९६० में संकलित कर 'योग' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया। यह बृहदाकार ग्रन्थ कदाचित् उनकी सर्वोत्कृष्ट सफल कृति है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के आत्मोन्नयनकारी प्रवचनों का समावेश है जो एक अभिजात सन्त, एक बहुश्रुत विद्वान् तथा एक महान् साधक का एकीकृत रूप था। जैसा कि पहले ही आभास कराया जा चुका है यह महान् ग्रन्थ हमें सनातन-धर्म का उसके शुद्ध तथा व्यावहारिक रूप में सन्देश देता है।
गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात् जब १९६५ में सत्संग तथा स्वाध्याय पर उनके लेख मरणोपरान्त पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए तो स्वामी जी ने उसमें परिशिष्ट के रूप में 'गुरुभक्ति का महत्व' तथा 'स्वाध्याय क्यों' को संयुक्त कर दिया। इन परिशिष्टों में उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया है कि एक विशिष्ट सन्त के साथ दीर्घकालिक सत्संग की चरम परिणति गुरु-शिष्य के दिव्य सम्बन्ध में होती है। इस भाँति सत्संग जिज्ञासु को जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा के एक निश्चित प्रक्रम में ले जाता है। स्वाध्याय भी साधक के लिए सर्वोपरि महत्त्व का है; क्योंकि आध्यात्मिक अध्ययन और पुनरध्ययन मात्र ही उसके मन में एक अमिट छाप छोड़ते हैं। स्वामी जी दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि अकेले सत्संग तथा स्वाध्याय व्यक्ति के सम्पूर्ण आन्तर स्वरूप को रूपान्तरित कर सकते हैं और यदि मानसिक स्थिति एक बार वास्तव में शुद्ध हो जाती है तो ध्यान का एक ही प्रयास व्यक्ति को निर्विकल्प-समाधि में पहुँचा देता है।
स्वामी जी के उपदेशों की एक पुस्तिका की आवश्यकता चिरकाल से अनुभव की जा रही थी। स्वामी प्रेमानन्द जी, जो स्वयं एक उच्च कोटि के सन्त हैं, ऐसी पुस्तिका को पूर्ण करने के अपने संकल्प को व्यक्त करने को बहुत पहले सन् १९५६ में स्वामी जी से मिले। अपने सजातियों के लिए करुणा से पूर्ण स्वामी जी के स्नेहमय शब्दों का प्रभाव पवित्र विलेपन अथवा पवित्र उपशामक तेल-सा होता है। प्रेमानन्द जी ने यह देख कर कि स्वामी जी के पवित्र ओष्ठों अथवा लेखनी से निःसृत शब्दों में आश्चर्यजनक शक्ति है परम पूज्य के कुछ उत्कृष्ट लेखों तथा प्रवचनों का संकलन कर सन् १९६८ में उन्हें निम्नांकित सोलह अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया : ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, विराट् की पूजा, अन्तःकरण, सन्तोष, करुणा, दृढ़ निश्चय, चरित्र, ब्रह्मचर्य, दानशीलता, शिष्टता तथा सौजन्यता, वाक्शक्ति का संरक्षण, चेतावनी, धारणा तथा ध्यान, संसिद्धि, प्रधान-प्रस्तर तथा आह्वान। इन सोलह प्रकरणों पर स्वामी जी के सन्देश मानो चिदानन्द के व्यक्तित्व की सोलह दिव्य पंखुड़ियाँ हों। यह 'चिदानन्दास क्रिज्म' (Chidananda's Chrism- 'चिदानन्द-चन्द्रिका') नामक पुस्तक परम पूज्य को उनके इक्यावनवें जन्मदिवस को भेंट की गयी। इस पुस्तिका के पृष्ठों के माध्यम से स्वामी जी का प्रमुख सन्देश है शरीर के 'प्रत्येक श्वास के साथ करुणा तथा प्रेम का स्पन्दन ।'
यह लेखक भी सन् १९७१ में हैदराबाद में आयोजित दिव्य जीवन सम्मेलन के सत्रों में सम्मिलित हुआ। उसने स्वामी जी के वहाँ के भावोद्गारों का संकलन तैयार किया। 'चिदानन्द स्पीक्स' (Chidananda speaks- 'चिदानन्द उवाच') नामक यह पुस्तिका चतुर्थ अखिल उड़ीसा दिव्य जीवन सम्मेलन, भवानीपटना में पूज्य चरण स्वामी जी को निःशुल्क वितरणार्थ भेंट की गयी। आलोच्य प्रवचनों में स्वामी जी ने इस मूलभूत सत्य पर बल दिया है : "भगवान् पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम भगवान् में हैं। भगवान् हममें हैं। यह शत-प्रतिशत सत्य है।"
उनके छप्पनवें जन्मदिवस के पुण्य अवसर पर 'मेसेज टु मैनकाइण्ड' (Message to Mankind-' मानवता से') पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें उनके भाषणों 'मानवता से', 'योग', 'गुरु तथा शिष्य', 'साधना तथा धर्म' तथा 'दिव्य जीवन' का समावेश है। वह इन प्रवचनों में हमसे इहलौकिक जीवन की महती अर्थवत्ता को भलीभाँति समझने की माँग करते हैं। वह बल देते हैं कि जीवन तथा साधना समानार्थी होनी चाहिए। स्वयं जीवन एक आध्यात्मिक प्रक्रम होना चाहिए। हमारी सम्पूर्ण सत्ता यज्ञ की भावना से सन्तृप्त होनी चाहिए।
स्वामी जी के उपदेश किन्हीं विशेष अवसरों पर विमोचित उनकी लघु पुस्तिकाओं द्वारा भी हमें ज्ञात होते हैं। ऐसी ही एक रचना 'स्वामी कृष्णानन्द' है। स्वामी जी आश्रम में श्रद्धेय कृष्णानन्द जी के साथ तीस वर्षों से अधिक समय तक रहे हैं तथा गुरुदेव के जीवनकाल से ही ये दोनों आध्यात्मिक महारथी दिव्य इकाई के आकाशदीप माने जाते थे। स्वामी जी कृष्णानन्द जी को वस्तुत: अपनी ही आत्मा समझते हैं। जब इस अभ्याससिद्ध वेदान्ती की स्वर्णजयन्ती सन् १९७२ में मनायी गयी तो स्वामी जी ने एक पुस्तिका लिखी जिसमें उन्होंने कृष्णानन्द जी को एक तितिक्षु, तपस्वी, जितक्रोध तथा ज्ञानी के रूप में चित्रित किया। गुरुदेव के वरिष्ठ शिष्यों के साथ स्वामी जी कैसा सम्बन्ध रखते हैं, इसे यह पुस्तिका सूचित करती है। इसी भाँति श्रद्धेय माधवानन्द जी के साठवें जन्मदिवस के पुण्य अवसर पर विमोचित एक 'स्मारिका' के अपने एक नूतन लेख में उन्होंने यह घोषित कर अपना सम्मान-भाव व्यक्त किया है कि माधवानन्द जी क्रोध के उन्मूलन के विषय में उनसे भी बढ़ कर हैं। स्वामी जी इस प्रकार हमें अपने वैयक्तिक उदाहरण द्वारा शिक्षा देते हैं कि हमें किस प्रकार अपने चतुर्दिक् के भद्र व्यक्तियों के प्रति विनम्रता तथा प्रचुर प्रशंसोक्ति के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए।
सन् १९७३ में स्वामी जी की पुस्तक 'पाथ टु ब्लेसेडनेस' (Path to Blessedness - 'मुक्तिपथ') का विमोचन हुआ। यह पुस्तक हमें महर्षि पतंजलि के अष्टांग-योग का सार प्रस्तुत करती है। उनके ही शब्दों में, "यह (पुस्तक) आत्मसंयम, मनोनिग्रह, धारणा तथा ध्यान के द्वारा अन्तरात्मा के साक्षात्कार का सरल निरूपण 81 ^ prime prime उन्होंने अपने प्रवचनों में धारणा, ध्यान तथा समाधि की अधिक विकसित अवस्थाओं की अपेक्षा यम तथा नियम के आधार की ओर अधिक ध्यान दिया है। एक निपुण योगाभ्यासी होने के कारण उन्होंने आधुनिक मानवों की मूलभूत त्रुटियों को बहुत ही यथार्थ रूप में देखा है और इसलिए योग में उनकी सफलता के लिए व्यावहारिक प्रतिकारक प्रस्तुत किया है।
स्वामी जी ने अपनी पुस्तक 'ए गाइड टु नोबल लिविंग' (A Guide to Noble Living - 'महान् जीवन की पथ-प्रदर्शिका') में साधकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया है कि सम्पूर्ण जीवन ही योग है। योग नियतकालिक ध्यान तक ही सीमित नहीं है। यह शरीर दूसरों के सेवार्थ है। उनके लिए व्यावहारिक जीवन का प्रचुर मानवीकरण तथा दिव्यीकरण वास्तविक योग है। अतः वह लक्ष्य तक पहुँचने का उपयुक्त मार्ग दर्शाते हैं: "नैतिकता से आरम्भ कर सन्तत्व से गुजरते हुए ईश्वरपरायणता की पराकाष्ठा पर पहुँच जायें 1 ^ prime prime उनका कथन है कि दिव्य जीवन स्वभावतः ही योग पर आधारित तथा वेदान्त से अनुप्राणित जीवन है। वह साधकों से अपने अन्दर इस प्रकार की योगाग्नि को सदैव प्रज्वलित बनाये रखने का अनुरोध करते हैं। वह व्यावहारिक साधना पर अपने प्रवचन में निम्नांकित संकेत प्रस्तुत करते हैं:
(१) मन को कभी भी पूर्णतः बहिर्मुखी न होने दें।
(२) सतत विचार तथा उन शास्त्रों के सतत स्वाध्याय द्वारा यथोचित मनोभाव उत्पन्न करें जो संसार की असारता, सांसारिक पदार्थों की निरर्थकता तथा समग्र सृष्टि के नश्वर स्वरूप को दर्शाते हैं।
(३) मन को भगवान् पर केन्द्रित रखें। सदा भगवन्नाम का मानसिक जप करें। नाम-स्मरण करें।
(४) जब वृत्ति उठे तो उस ओर ध्यान न दें, उसे विलीन हो जाने दें।
(५) जप, कीर्तन, प्रार्थना, सत्संग तथा स्वाध्याय के द्वारा वासना को समाप्त करें।
(६) वासनाओं को कम करें तथा संकल्पशक्ति को बलवान् बनायें ।
(७) मन को समझें, मन का विश्लेषण करें तथा इस यन्त्रावली का सम्यक् परिचय तथा उसे नियन्त्रित करने की जानकारी प्राप्त करें।
(८) कामनाओं के प्रकट होने पर उन्हें पूर्ण न करें।
(९) अन्तरावलोकन तथा आत्मविश्लेषण करें तथा ऐसा करते समय अपने प्रति कठोर रहें।
(१०) सत्यता, करुणा तथा शुचिता-ये वे मूलभूत बातें हैं जिन पर भौतिक तल की सभी प्रवृत्तियाँ अवलम्बित होनी चाहिए।
(११) मिताचारी जीवन यापन करें।
वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्यस्त रहने वाले आधुनिक लोगों के लिए आत्म-संसूचन का दिव्य मनोविज्ञान निर्धारित करते हैं: "अपने खोये हुए पैतृक अधिकार को, अपने सत्स्वरूप को स्मरण करें तथा बार-बार उसका पुनः दावा करें।" वह साधना के पूर्ण क्रम के रूप में निम्नांकित तीन बातों का सुझाव देते हैं :
(१) कोई भी कार्य आरम्भ करने से पूर्व यह कल्पना करें तथा अनुभव करने का प्रयास करें कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं वह प्रभु का भव्य भजन है।
(२) कार्य करते समय, समय-समय पर यह अनुभव करने का प्रयास करें कि वह कार्य आपके द्वारा नहीं हो रहा है, कि आप निमित्त मात्र हैं और प्रभु की सर्वशक्तिमती शक्ति ही आपके माध्यम से कार्य कर रही है।
(३) जब आप कार्य समाप्त कर चुकें तो उसे प्रभु को अर्पण के रूप में करें। आपका अन्तिम कार्य पूरे मन से अर्पण-कृष्णार्पण हो।
परम श्रद्धेय स्वामी जी ने 'ए गाइड टु नोबल लिविंग' (A Guide to Noble Living) में जो-कुछ कहा है, उसे संक्षिप्त रूप में 'दि पिल्ग्रिम रोड' (The Pilgrim Road) में प्रस्तुत किया गया है जिसका विमोचन उनके हीरक जयन्ती-महोत्सव के पुण्य अवसर पर किया गया था।
विश्वभर के लाखों भक्तों से निकट का वैयक्तिक सम्पर्क बनाये रखने के लिए स्वामी जी प्रथम तो 'विज़डम लाइटू' (Wisdom Light) पत्रिका में 'परमाध्यक्ष की ओर से' शीर्षक के अन्तर्गत तथा तत्पश्चात् 'द डिवाइन लाइफ' (The Divine Life) पत्रिका में 'शिवानन्दाश्रम पत्र' शीर्षक के अन्तर्गत खुले पत्र लिखते रहे हैं। स्वामी जी ने इन पत्रों के माध्यम से भक्तों को अपनी यात्राओं की सभी घटनाओं से पूर्णतः अवगत बनाये रखा है। इन पत्रों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष है साधकों से उनके आशु विकास के लिए उनका अपरोक्ष प्रेरणाप्रद आग्रह। इसमें वह विश्व के विभिन्न भूभागों के अपने यात्राकाल में अन्य महान् आध्यात्मिक विभूतियों के साथ किये हुए अपने सत्संग का लाभ भी उन्हें देते हैं। इनमें से कुछ पत्रों का संकलन सन् १९७४ में 'एडवाइस आन स्पिरिट्यूअल लिविंग' (Advice on Spiritual Living) शीर्षक के अन्तर्गत किया गया था।
जिज्ञासुओं को अपने साधना-काल में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक 'गाइड लाइन्स टु इल्यूमिनेशन' (Guidelines to Illumination - 'ज्योतिपथ की ओर') में, जिसका विमोचन १९७३ में हुआ था, उन्हें इन बाधाओं को पार करने के लिए अनेक प्रभावशाली विधियाँ निर्धारित की। इस पुस्तक के विषय का चयन स्वामी जी के भाषणों से किया गया है जिनमें से अधिकांश भाषण सन् १९६९-७० में विदेश में दिये गये थे। स्वामी जी इस पुस्तक में प्रबोधित करते हैं: "दिव्यता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः निरन्तर साधना द्वारा उसे प्रस्फुटित करें। भगवत्प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य से रहित मानव-जीवन व्यर्थ है, सार-रहित है।" उन्होंने जिज्ञासुओं तथा योगाभ्यासियों को मोहक सिद्धियों से दूर रहने के लिए सावधान किया है। मानव जाति के लिए उनका उत्कृष्ट उपदेश है : "इस विश्वरूप ईश्वर को प्रणाम करने के लिए सूर्योदय से पूर्व ही निद्रा त्याग दें। दैनिक चर्या आरम्भ करने से पूर्व उसे प्रणाम करें, श्रद्धा से झुक जाये। पूजा-भाव से दिवस को भर दें।"
स्वामी जी ने लोगों तक सनातन धर्म का शाश्वत सन्देश पहुँचाने के लिए भारतवर्ष के कोने-कोने तथा महत्त्वपूर्ण स्थानों तक पहुँचने का अथक प्रयास किया है। सन् १९७५ के अन्तिम दिनों में उन्होंने भंजनगर के निकट की ग्रामीण जनता के सम्मुख कतिपय भाषण दिये तथा उन्हें अनुप्राणित करने वाली आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। इन भाषणों का उड़िया-भाषान्तर भंजनगर की दिव्य जीवन संघ शाखा ने 'साधना' नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। इन भाषणों में उन्होंने भोले-भाले ग्रामीण लोगों से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने का अनुरोध किया है। वह उनसे अपने सामाजिक जीवन के त्याग की माँग नहीं करते हैं।
स्वामी जी ने प्राच्य तथा पाश्चात्य जगत् के असंख्य जिज्ञासुओं को अतीव कृपापूर्वक शक्तिशाली मन्त्र-दीक्षा से दीक्षित किया है और इस प्रकार उन्हें दिव्य नाम की साधना के लिए आवश्यक साधन प्रदान किया है जो वर्तमान युग में सर्वाधिक प्रभावकारी आध्यात्मिक अस्त्र है। साधना के इस सन्दर्भ में उनका प्रवचन हिन्दी में 'एडवाइस टु द इनिशिएटेड् डिसाइपल्स' (Advice to the Initiated Disciples -'नवदीक्षितों को उपदेश' नाम से प्रकाशित किया गया है। उन्होंने शिष्यों को अपनी दैनिक साधना में निम्नांकित बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा है :
(१) यह दृढ़ विश्वास रखें कि कलियुग में मन्त्र जप से भगवत्साक्षात्कार होता है।
(२) यह जान लें कि गुरु भगवान् है। नाम तथा नामी अभिन्न हैं।
(३) प्रतिदिन न्यूनातिन्यून ग्यारह माला जप करें।
(४) दैनिक जप को कभी बन्द न करें।
(५) इष्ट-मन्त्र को गुप्त रखें।
(६) सप्ताह में एक बार प्रत्येक मन्त्र-दीक्षा-दिवस को आंशिक उपवास करें। वर्ष में एक बार मन्त्र-दीक्षा तिथि को पूर्ण उपवास करें।
(७) सद्गुणों का अर्जन तथा दुर्गुणों का उन्मूलन करें।
(८) अपने इष्ट-देवता का दर्शन सभी देवी-देवताओं में करें तथा यह जानें कि ईश्वर साकार तथा निराकार दोनों ही है।
(९) ईश्वर तथा गुरु की विद्यमानता सदा अनुभव करें।
(१०) प्रत्येक दीक्षित शिष्य को शुचिता तथा निष्कल्मषता का अभ्यास करना चाहिए।
खुर्दा रोड में आयोजित एक क्षेत्रीय दिव्य जीवन सम्मेलन में स्वामी जी ने हिन्दी में 'ध्यान के सिद्धान्तों तथा प्रविधि' पर श्रृंखलाबद्ध तीन भाषण दिये। इन भाषणों में उन्होंने साधकों से आचारिक पवित्रता तथा मोक्ष की ज्वलन्त कामना बनाये रखने का अनुरोध किया। तभी ध्यान के लिए अपनायी गयी प्रविधि फलप्रद होगी। स्वामी जी ने कहा- "त्रिकाल में विद्यमान सच्चिदानन्द-सागर को मन में स्पष्ट रूप से देखने का प्रवास करें। अपने सभी वैयक्तिक गुणों से युक्त आपके इष्टदेव लहर के रूप में इस सागर से प्रकट होते हैं। उनके साकार रूप का दर्शन तथा उनके मन्त्र का जप करें। अपने सभी विविध विचारों को उनके चरण कमलों में मानसिक रूप से अर्पित करें। ध्यान की समाप्ति पर अनुभव करें कि आपके इष्टदेव एक बार पुनः उस सच्चिदानन्द-सागर में विलीन हो गये हैं। कुछ क्षणों तक मौन रखें। तत्पश्चात् सन्तुलित मन से ध्यान-कक्ष से बाहर निकलें। इस अभ्यास के तुरन्त बाद ही सांसारिक प्रवृत्तियों में न उलझ जायें। इस
ध्यानाभ्यास को आरम्भ करने से पूर्व कुछ क्षणों तक अपने गुरु के रूप पर धारणा करें, उनके आशीर्वाद की याचना करें और तब अपने इष्टदेव पर ध्यान करना आरम्भ कर दें।" हीरक जयन्ती-समारोह के अवसर पर श्री सी. एस. दास द्वारा 'ध्यान-साधना' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इन भाषणों के उड़िया-भाषान्तर में इन संकेतों का समावेश किया गया है।
एक लघु पुस्तिका 'दि आइ आव द हरिकेन' (The Eye of the Hurricane -'प्रभंजन-नेत्र') जिसमें लास ऍजिलेस में दिये गये स्वामी जी के प्रवचन का समावेश है, का विमोचन सन् १९७६ में हुआ। इसमें वह उपदेश देते हैं कि जीवन मृत्यु की ओर मन्द गति से चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, अतः इसका पूर्ण सदुपयोग होना चाहिए। जीव को स्वर्णिम कुंजी दी गयी है और यह स्वर्णिम कुंजी एक विलक्षण नियम है जो सारे ब्रह्माण्ड को नियन्त्रित किये है जिसे कर्म का नियम कहते हैं। स्वामी जी जिज्ञासुओं से अनुरोध करते हैं कि अपने बहिर्गामी स्वभाव का परिवर्तन करें। उसके सम्पूर्ण आचरण के आदर्श के स्थान पर नवीन आचरण के आदर्श को स्थापित करें जो आध्यात्मिक अज्ञान का विषघ्न हो। मन के अशान्त स्वभाव को योगाभ्यास द्वारा अनुशासित किया जाता है। मन के सम्मुख एक निश्चित केन्द्र-बिन्दु प्रस्तुत किया जाता है। प्रारम्भ में यह केन्द्र-बिन्दु एक दिव्य पदार्थ, निराकार सत्ता की साकार कल्पना होता है। यहाँ मन समाहित तथा दिव्य बन जाता है। उस पूर्ण संविलयन की स्थिति में रहस्यमयी समाधि की अवस्था आती है। फिर मन अमन बन जाता है। परम सत्ता में मन का विलयन ही मोक्ष है। यह केन्द्र-योग है, प्रकाशपूर्ण चैतन्य-योग है। हठयोग तथा ध्यान की अनेक प्रविधियाँ परिधि के योग तथा वृत्त-क्षेत्र के योग हैं; किन्तु इस केन्द्र-योग ईश्वर में केन्द्रीभूत तथा सत्य में केन्द्रीभूत होने की चेतना के योग के लिए किसी विशेष स्थान, धूपबत्ती, मखशाला अथवा वेदी की आवश्यकता नहीं है। यह नवं युग का योग है जिसका उपदेश चिदानन्द आधुनिक मानव को देते हैं।
स्वामी जी की 'लेक्वर्स आन राजयोगा' (Lectures on Raj Yoga) पुस्तक 'पाथ टु ब्लेसेडनेस' (Path to Blessedness -' मुक्तिपथ') पुस्तक की मूल्यवान सम्पूरक है। इस पुस्तक में योग-शान्ति-निकेतन, बेरूत में सन् १९७३ की वसन्त ऋतु में आध्यात्मिक साधकों की एक टोली के सम्मुख दिये हुए प्रवचनों का समावेश है। इसमें उन्होंने पतंजलि के योगसूत्रों की कोई टीका अथवा व्याख्या नहीं प्रस्तुत की है, वरन् योग के केवल व्यावहारिक उपदेश दिये हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति स्वयं अपना मनश्चिकित्सक बन सकता है।
सच्चे जिज्ञासुओं को दिये गये स्वामी जी के उपदेशों तथा सन्देशों को 'इटर्नल मेसेजेज' शीर्षक के अन्तर्गत उनकी हीरक जयन्ती के मंगलमय अवसर पर प्रकाशित किया गया है। उनका प्रमुख उपदेश, उनके सन्देशों का मूल-स्वर प्रत्येक व्यक्ति को सर्वशक्तिमान् प्रभु की सर्वव्यापिता अनुभव करने के लिए आह्वान है। वह सदा ही लोगों को पूजा के मनोभाव से, ईश्वर को समर्पण-भाव से कार्य करने का उपदेश देते हैं। यही भारतवर्ष का उसके प्रेरित दूतों के माध्यम से दिया गया मानव को मोक्ष प्रदान करने वाला मन्त्र है, शाश्वत सन्देश है।
स्वामी जी के कुछ उत्कृष्ट उपदेशों को श्री वी. एल. नागराज ने १९७४ में चिदानन्द हीरक जयन्ती-माला के अन्तर्गत पाँच पुस्तिकाओं में सम्पादित किया है। स्वामी जी की शाश्वत दिव्य चेतना, कर्मयोग के रहस्य की मार्गदर्शक रूपरेखा, व्यावहारिक वेदान्त पर उनके उपदेश, शुचिता के लिए प्रार्थना में उनकी आस्था तथा गम्भीरतम गुरुभक्ति को इस माला में अपूर्व ढंग से सँजोया गया है जो पाठकों को एक अर्थ में पूज्यास्पद स्वामी जी के उपदेशों का सारतत्त्व प्रदान करती हैं।
'पाथ बियान्ड सारो' (Path Beyond Sorrow) में पाश्चात्य जगत् के जिज्ञासुओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शन समाविष्ट है। स्वामी जी ने सन् १९६० में गुरुदेव के निजी प्रतिनिधि के रूप में नयी दुनिया (अमरीका) में कई भाषण दिये तथा उस भौतिकवाद-प्रधान वातावरण में आध्यात्मिक हलचल उत्पन्न कर दी। इन प्रवचनों ने पुस्तक के कलेवर का रूप ले लिया जो योग-सम्बन्धी सभी भ्रान्त धारणाओं को विदूरित करती तथा स्वामी जी के अन्तर्ज्ञानोपलब्ध अनुभव की दृष्टि से उस (योग) का प्रमुख अर्थ प्रस्तुत करती है। वह मानते हैं कि योग एक मनोभौतिक विज्ञान मात्र नहीं है, अपितु यह अध्यात्म-विज्ञान है जिसका यदि अभ्यास किया जाय तो यह निम्न प्रकृति को दिव्य चेतना में रूपान्तरित कर देता है।
योगासन मूलार्थ में योग नहीं है। तथापि वे योग के अंगों में से एक हैं। ये जिज्ञासु को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए तैयार करते हैं। स्वामी जी ने ये निर्देश अपनी पुस्तक 'प्रैक्टिकल गाइड टु योगा' (Practical Guide to Yoga) में अपनी साठ वर्ष की आयु में दिये थे। उन्होंने इस वृद्धावस्था में भी इस सन्दर्शिका के लिए योगासनों का यथावत् प्रदर्शन किया। उन्होंने दर्शाया कि खड़े हो कर तथा बैठ और लेट कर की जाने वाली शिथिलन को सभी प्रविधियाँ मनुष्य के अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय कोशों में किस प्रकार सामंजस्य उत्पन्न करती हैं।
स्वामी जी की शिक्षाएँ पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में प्रकाशित हुई हैं, उन्हें टेप (फीते) तथा ग्रामोफोन रेकाडों पर अभिलेखन किया गया है तथा वे आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यमों से प्रसारित की गयी हैं। स्वामी जी ने गुहाओं तथा आश्रमों में उपदेश दिये हैं। विशाल जन-समूह के सम्मुख ओजस्वी भाषण दिये हैं तथा जिज्ञासुओं के साथ की भेंटवार्ताओं में ज्ञान-मुक्ताएँ प्रदान की हैं। उन्होंने धर्म-परिषद् में मूल सिद्धान्तों पर भाषण दिये, शिवानन्द भ्रातृ संघ के गुरुभाइयों को उन्नयनकारी सत्संगों में सम्बोधित किया, रूढ़िवादी विचारकों को शास्त्रों के गुह्य अर्थ को व्यक्त किया तथा सर्वोपरि बात यह है कि जिन्हें उनके उपदेशों की आवश्यकता थी तथा जिन्होंने उनसे सान्त्वना की याचना की उन सभी लोगों को अपने वैयक्तिक सन्देश तथा आशीर्वाद सम्प्रेषित किये। निस्सन्देह वह विश्व के पथप्रदर्शक हैं।
स्वामी के उपदेश आश्रमों तथा शिष्यों तक ही सीमित नहीं हैं। चिदानन्द का भण्डार जाति, पन्थ, धर्म तथा लिंग का विचार किये बिना सभी लोगों के लिए खुला है; वह सभी जिज्ञासुओं के लिए समान रूप से उत्कण्ठित हैं। चिदानन्द के उपदेश वितण्डावादी अनर्थक शब्दों से बोझिल नहीं हैं। उनमें पण्डिताऊ संस्कृत उद्धरणों का विरामचिह्न नहीं लगा है। उनका झुकाव आत्मज्ञानपरक निराधार कल्पनाओं की दिशा में नहीं है। चिदानन्द-साहित्य घनीभूत ज्ञान से निस्सृत नित्य शुद्ध पावन सरिता है, हिमालय के शीर्षस्थ सन्त शिवानन्द से निर्गत वास्तविक ज्ञान-गंगा है। यह विश्वभर के लाखों लोगों की पिपासा को शमित करती हुई निरन्तर आगे-आगे प्रवाहित होती रहती है।
चिदानन्द अपने को अगम्य ऊँचाइयों पर प्रतिष्ठित नहीं रखते हैं। वह प्रत्येक सामान्य मर्त्य मानव के मित्र तथा पथप्रदर्शक के रूप में उसके स्तर तक नीचे उतर आने को, झुकने को सदा तैयार रहते हैं। उनके भाषण औपचारिक धर्मोपदेशों की भाँति नहीं होते हैं। वे निरपवाद रूप से सभी लोगों के प्रति अपरोक्ष, निष्कपट अभ्यर्थनाएँ हैं। कहा जाता है कि उत्कृष्ट कविता व्यक्ति के समझने के पूर्व ही अपना भाव प्रकट कर देती है। ऐसा ही चिदानन्द का भाषण भी करता है। बौद्धिक प्रक्रिया द्वारा हृदयंगम किये जाने से पूर्व ही वह हृदय में प्रवेश कर जाता है तथा जिज्ञासु श्रोताओं तक तत्काल सन्देश पहुँच जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके ज्ञानमय शब्द पूर्ण अनुभूति से प्रकट होते तथा प्रेम और करुणा के दबाव के कारण फूट निकलते हैं।
चिदानन्द ने अपना कोई मत नहीं स्थापित किया है। उन्होंने अपने को भगवान् तथा गुरुदेव के हाथों का पूर्ण व्यक्तिकता-रहित उपकरण बना डाला है। वह अपने सभी लेख, भाषण तथा प्रार्थनाएँ गुरुदेव के नाम से आरम्भ करते हैं। अपनी नवीनतम रचना 'प्रैक्टिकल गाइड टु योगा' (Practical Guide to Yoga) में 'मेरे योगी गुरु ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी शिवानन्द जी महाराज के चरणों को श्रद्धामय नमस्कार' जैसे शब्दों से आरम्भ तथा अपनी प्राचीनतम रचना 'लाइट् फाउण्टेन' (Light Fountain -'आलोक-पुंज') के 'यहाँ आपके गुरु, आपके स्वामी, विश्व के सन्देशवाहक तथा नागरिक हैं' जैसे शब्दों से समापन किया है। सदा तथा सभी अवसरों पर ऐसा सम्बोधन करने की उनकी स्थायी शैली रही है। वह अपने निजी उदाहरण द्वारा समर्पण की सच्ची भावना की शिक्षा देते हैं। उनके अपने ही शब्दों में "शिवानन्द की अलक्ष्य आध्यात्मिक उपस्थिति अब भी मेरा पथप्रदर्शन कर रही है।"
उनके सभी लेखों में एक सामान्य विशिष्टता पायी जाती है। वह सेवा तथा परोपकार के स्वर से आरम्भ करते हैं, भगवन्नाम के स्मरण पर बल देते हैं, जिज्ञासुओं से योग के द्वारा विचार-शक्ति के अध्यात्मीकरण का अनुरोध करते हैं तथा अपने सन्देश को वेदान्त के परम सत्य की ओर ले जाते हैं। इसका समग्र प्रभाव सदा ही आश्चर्यकर, पराभूतकारक तथा परम सन्तोषजनक होता है।
सेवा, प्रेम, दान, पवित्रता, ध्यान, साक्षात्कार; शिवानन्द के ये सारगर्भित प्रभावशाली उपदेश चिदानन्द की सभी रचनाओं में निविष्ट हैं। भगवान् को सतत स्मरण करें। सद्गुणों का अर्जन करें। सभी प्रवृत्तियों का अध्यात्मीकरण करें। गुरुदेव के उपदेशों के ये तीन मूल तत्त्व उनके सभी लेखों में रजत-सूत्र की भाँति सन्निविष्ट हैं तथा अन्तस्थित भगवान् के परम सरल तथा ऋजु मार्ग को प्रकाशित करते हैं।
द्वादश अध्याय
दिव्य जीवन
"सर्वगुहातमं भूयः शृणु मे परमं वचः
-सम्पूर्ण गोपनीयों से भी अतिगोपनीय मेरे परम रहस्यमय वचन को फिर सुनों" (गीता : १८/६४) ।
स्वामी चिदानन्द का इतिवृत्त मानव-व्यक्तित्व के पूर्ण दिव्यीकरण का इतिवृत्त है। यह मौन सेवा तथा पूर्ण अनात्मशंसा का इतिवृत्त है। अतः हिमालय का यह अप्रतिम सन्त अपने वैयक्तिक अनुभव के गम्भीर प्रमाण तथा अपरोक्ष अन्तर्ज्ञानोपलब्ध बोध के आधार पर जिज्ञासु-जगत् में यह घोषित कर सका, "योग मात्र निर्विकल्प-समाधि की अवस्था में ही नहीं है। यह जीवन के प्रत्येक क्षण में है।" उनका जीवन निष्कलंक ईश्वरपरायणता से प्रतिक्षण प्रदीप्त रहता है।
चिदानन्द का जीवन पवित्र सेवा की गाथा है। सेवा तथा आत्मत्याग उनके जीवन की प्रमुख विशिष्टताएँ रही हैं। उनका संस्कार ऐसा था कि श्रेष्ठ आध्यात्मिक सद्गुण उनके लिए सहज संकल्प-व्यापार थे। इस भाँति इस नि:सीम करुणापूर्ण सन्त ने अपनी किशोरावस्था में ही उन भाग्यहीन कुष्ठियों के पिता तथा चिकित्सक होने के भयजनक कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया जिन्हें उनके सभी सजातियों ने ठुकरा दिया था और जिनको वे घृणा करते थे। औदार्य, पवित्रता तथा करुणा उनमें सहज रूप से आये। भौतिक समृद्धिमय जीवन के विचारों से वह कभी भी प्रलुब्ध नहीं हुए। उनका जन्म एक सम्पन्न परिवार में हुआ तथा राजकुमारों की भाँति उनका पालन-पोषण हुआ; किन्तु धन-सम्पत्ति तथा सांसारिक प्रतिष्ठा उनके लिए अर्थहीन थी। यौवनावस्था में भी वह इन्द्रियों के पाश से बहुत ऊपर थे। सेवा तथा आत्मत्याग ही उनके सुख-साधन थे। सन्तों की संगति ही उनकी एकमात्र लालसा थी। ध्यान उनकी एकमात्र वासना थी। पूजा ही उनका एकमात्र आमोद था।
इस जन्मजात सिद्ध को अपने नवयौवन-काल में यह अनुभव हुआ कि वह संसाराग्नि में झुलस रहे हैं। अतः उपयुक्त समय आते ही उन्होंने तत्काल अपना घरबार त्याग दिया। वह एक पूर्णिमा के पुण्य दिवस को ऋषिकेश में पावनी गंगा के तट पर अपने गुरुदेव से मिले। उन्होंने गैरिक परिधान धारण कर लिया तथा पुरातन संन्यास-आश्रम से सम्बद्ध हो गये। एक दशक से अधिक समय तक वह उग्र सेवा तथा साधना में निमग्र रहे तथा एक ज्ञानी के रूप में विभासित हुए। इसके आगामी दशक में गुरुदेव के जीवनकाल में उन्होंने नयी दुनिया में योग तथा वेदान्त का सन्देश पहुँचाया। वहाँ से वापस आ कर वह स्वेच्छा से एक एकाकी परिव्राजक संन्यासी का जीवन-यापन करते हुए एकान्तवास में निमग्न हो गये। वह संन्यासाश्रम से भी उदासीन हो चले। वह भगवान् पर निर्भर रह कर ईश्वरीय चेतना की भूमिका में आनन्दपूर्वक निवास करते हुए सभी पाशों से मुक्त हो एक अवधूत की भाँति स्वच्छन्द विचरण करते थे।
इस अवस्था में भगवदिच्छा उन्हें लोक-संग्रह की, उत्कृष्ट आध्यात्मिक सेवा की भूमिका में वापस लायी। गुरुदेव स्वामी शिवानन्द ने अपना भौतिक कलेवर त्याग दिया तथा वह परम सत्ता में विलीन हो गये। अतः गुरुदेव के दिव्य मिशन के नेतृत्व का कार्य उनके चुने हुए शिष्य के कन्धों पर पड़ा। इस भाँति संसार का त्याग करने वाला व्यक्ति आधुनिक जगत् में सर्वाधिक सक्रिय धार्मिक कार्यकर्ता बना।
चिदानन्द सभी समयों तथा सभी अवसरों पर अश्रान्त सेवा करते हैं। वह प्रभु की इस विश्व-रूप में सेवा करते हैं। वह अपने गुरुदेव के दिव्य मिशन के माध्यम से सेवा करते हैं। वह राममय जगत् में निवास करते हैं। राम उनके जीवन में क्योंकर आये, यह प्रत्येक जिज्ञासु के लिए एक शिक्षाप्रद पाठ है। वह उनके जीवन में उनकी बाल्यावस्था में कोदण्ड राम की मूर्ति के रूप में आये जिनकी वह पूजा करते तथा जिनमें अपनी पूर्ण सत्ता रखते थे। एक परवर्ती अवस्था में वह उनके पास हतभाग्य कुष्ठियों के रूप में आये। तत्पश्चात् एक ऐसा समय आया जब वह रामदास के उत्प्रेरित शब्दों के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। तदनन्तर रामकृष्ण परमहंस का जीवन अपनी ओर संकेत करते हुए एक आदर्श के रूप में उनके सम्मुख दिखायी पड़ा। सन्तों तथा रहस्यवादियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अन्त में भगवान् ने अपने सद्गुरु के रूप में उन्हें दर्शन दिया। शिवानन्द उनकी सत्ता में ही प्रवेश कर गये। वह गुरुभक्ति से आपूरित हो उठे। शिवानन्द उनमें वास करते थे और वह शिवानन्द में वास करते थे। दोनों मिल कर एक बन गये। स्वामी कृष्णानन्द जी के शब्दों में: "उन्होंने (चिदानन्द ने) श्री गुरुदेव से जो रिक्थ आत्मसात् किया है, वह शतप्रतिशत है। हमें उनमें गुरुदेव के सभी चमत्कारात्मक तथा आश्चर्यकारक गुण दृष्टिगोचर होते हैं।”
'सर्वं राममयं जगत्', 'सर्वं विष्णुमयं जगत्', 'वासुदेवः सर्वम्', 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' - ये उनके जीवन के सूत्र तथा जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों के नुसखे हैं। वह समग्र विश्व को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। यह संसार गुरु है। जीवन शिष्यत्व है। अतः व्यक्ति को अपना जीवन संसार की सेवा करने तथा स्वयं संसार से ज्ञान ग्रहण करने के लिए यापन करना है। यह धर्म है जो व्यक्ति को मोक्ष तक पहुँचाता है। यही मानव के प्रति चिदानन्द के सन्देश का मूल-भाव है। वह इस सन्देश को अपने व्यक्तिगत उदाहरण तथा गूँजने वाले आदेशों के माध्यम से सम्प्रेषित करते हैं। अतः उनमें वर्तमान गुरुपन की भावना ने विनम्र शिष्यत्व के जीवन को वरण किया है। वह अपने को सदा गुरुदेव का सेवक मात्र मानते हैं। वह अपने शिष्यों को गुरुदेव का शिष्य मानते हैं। इतना ही क्यों, वह उन्हें साक्षात् नारायण समझते हैं। वह आधुनिक काल के सन्तों के चूड़ामणि हैं, किन्तु वह सबके सामने नतमस्तक होते हैं। वह न केवल अपने गुरुजनों को अपितु अधमाधम लोगों को भी साष्टांग प्रणाम करते हैं।
वह इस पार्थिव जगत् के सभी प्राणियों की अक्षय करुणा के साथ सेवा करते तथा उनसे प्रेम करते हैं। जब वह आध्यात्मिक उपलब्धियों की पराकाष्ठा पर पहुँच गये तो निरर्थक बातों में करुणाजनक रूप से उलझे हुए अपने सजातियों के दयनीय दृश्य देख कर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सभी प्रकार की असुविधाओं तथा कठिनाइयों पर ध्यान न दे कर उन लोगों को मुक्त कराने के कार्य के लिए अपने को समर्पित कर दिया। उन्हें ज्ञात था कि लोग अज्ञानतावश भूलें करते हैं। अतः उन्होंने उन्हें न तो तुच्छ समझा और न उनकी भर्त्सना ही की। वरन् उनको ऊपर उठाने के लिए वे स्वयं प्रेम से नीचे झुक गये। उनका प्रेम निःसीम है जो पशुओं, पक्षियों तथा कीड़ों तक को अपने क्रोड़ में लेने के लिए फैला रहता है।
चिदानन्द सनातन धर्म की किरणें प्रसारित करने वाले एक शुद्ध क्रकच (प्रिज्म) हैं। नितान्त निष्कल्मष साधु व्यक्ति तथा साक्षात्कार-प्राप्त आत्मा होने से वह अमित आध्यात्मिक शक्ति से सम्पन्न हैं। उनकी उपस्थिति ही उन्नयनकारी अनुभव है। वह संघर्षरत जिज्ञासुओं के संशयों का निराकरण करती तथा उनमें नवीन आध्यात्मिक ओज अनुप्राणित करती है। उनके शिष्य अनेक हैं और ऐसे लोग तो असंख्य हैं जो यद्यपि उनसे दीक्षित नहीं है पर उन्हें अपना सद्गुरु मानते हैं। किन्तु यह प्रेम तथा करुणा का महान् स्वामी उन सबके मध्य में एक सामान्य साधक की भाँति विचरण करता है। वह जन्मजात सिद्ध है, किन्तु जिज्ञासु की भाँति आचरण करते रहते हैं।
असाधारण ऊँचाइयों पर आरोहण करने वाले ईश-मानवों ने मानव-मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बुद्ध अपने पीछे 'चार आर्य सत्य' तथा 'अष्टांगिक मार्ग' छोड़ गये। शंकराचार्य ने हमें परम सत्ता के पाठ का उत्तरदान किया। चैतन्य ने हमें नाम-संकीर्तन का आनन्दातिरेक प्रदान किया। शिवानन्द ने मानवता की सेवा, भक्ति, ध्यान तथा प्रबोध-रूप साधन-चतुष्टय प्रदान किया। इसी अविच्छिन्न परम्परा में, चिदानन्द सृष्टिकर्ता की खोज किसी अज्ञात रहस्यमय लोक में न कर स्वयं सृष्टि में ही खोजने का उपदेश हमें अपने भाव तथा कर्म द्वारा देते हैं। उन्होंने मानव को केन्द्र-योग, प्रकाशपूर्ण चैतन्य-योग, प्राणियों की सेवा तथा भगवदाराधन-योग का उत्तरदान किया है। वह नित्य निरन्तर पुजारी-भगवान् के सतत आराधक हैं। वह अपने सजातियों को दिव्य जीवन यापन करने के लिए भावोद्दीपक उपदेश देते हैं। वह अत्यधिक उत्कण्ठा तथा गम्भीर भाव से परामर्श देते हैं:
भगवान् के विराट् स्वरूप को नमस्कार करने के लिए प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्त में जग जायें। दिन का कार्य आरम्भ करने से पूर्व उन (प्रभु) के समक्ष श्रद्धा से नतमस्तक हों। शान्त चित्त तथा सुख-शान्ति तथा सन्तोष से पूर्ण रह कर दिनभर व्यवहार करें। इस संसार में कुछ भी गर्हित नहीं है। अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लायें। दुर्भाव त्याग दें। शत्रु को क्षमा कर दें। चिन्ता करना बन्द कर दें तथा अपने-आप मन्द-मन्द मुस्करायें। अनुभव करें कि यह समग्र संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है तथा आप इन सभी नामरूपों में उस ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। जीवन को योग में रूपान्तरित कर दें। सदाचारी तथा परोपकारी बनने का प्रयास करें। ईश्वर सरल लोगों के साथ चलता है, दुःखियों के प्रति अपने को उद्घाटित करता है, भद्र लोगों को विवेक प्रदान करता है तथा अहंकारियों से अपनी कृपा अलग रखता है। अतः अहन्ता त्यागें, सद्गुणों का अर्जन करें तथा मुक्त बनें। मन को सदा शान्त तथा निरुद्विग्न रखें। मन की बाधाओं पर विजय पाने का यही रहस्य है। बोलने से पूर्व अपने सभी शब्दों पर भली-भाँति विचार करें। इने-गिने शब्द ही बोलें। यह शक्ति को सुरक्षित रखेगा तथा मानसिक शान्ति तथा आन्तरिक शक्ति प्रदान करेगा। अपना प्रेम व्यक्त करें। इसे पुनः व्यक्त करें। इसे और भी पुनः व्यक्त करें। इसे एक बार पुनः और व्यक्त करें। मन को कभी भी पूर्णतया बहिर्गामी न होने दें। अपने मन के विजेता, अपनी वासनाओं के दमनकारी तथा अपने भाग्य के स्वामी बनें; क्योंकि आप ही स्वामी हैं।
गुरुदेव शिवानन्द आपको जगाने के लिए आये। भूल जायें कि आप यह नश्वर शरीर हैं। स्मरण रखें कि आप शुद्ध चेतना हैं। और अधिक निद्रा में न पड़े रहें। तृणवत् विनम्र बनें। सेवा करें। प्रेम करें। दान दें। शुद्ध बनें। ध्यान करें। आत्मसाक्षात्कार करें। भले बनें। भला करें। दयालु बनें। संवेदनशील बनें। दिव्यता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिव्यता को नियमित साधना द्वारा प्रकट करें। "ईशावास्यमिदं सर्वम्।" यह अखिल ब्रह्माण्ड ईश्वर से व्याप्त है। अतः मानव जाति की सेवा करें तथा दिव्यता की खोज करें।
ये चिदानन्द के सन्देश के स्वरचिह्न हैं। महान् गुरुदेव की भाँति वह समान रूप से बल देते हैं: "केवल विश्वास ही न कीजिए, वरन् वैसा बनिए तथा उसे जीवन में उतारिए।"
मानव-जीवन का महत् उद्देश्य भगवत्साक्षात्कार है। वृक्ष, पशु, पक्षी तथा कीड़े जन्म लेते तथा मर जाते हैं। उनका विकास नहीं होता है। उन्हें उनके स्रष्टा ने सद् तथा असद् में विवेक करने की चेतना से सम्पन्न नहीं किया है; किन्तु मानव-जीवन ईश्वर की अमूल्य देन है। किन्तु मानव-जीवन का पथ 'क्षुरस्यधारा' का पथ है। इन्द्रियों ने हमें अन्धा बना दिया है और हमारी चेतना का अपहरण कर लिया है। हमारे अनेक अन्धकूप हैं। जीवन के इस महान् तथा दुर्गम पथ में हमारी सँभाल करने तथा हमें सम्बल प्रदान करने के लिए यदा-कदा ईश्वर के सन्देशवाहक, हमारे मित्र तथा पथप्रदर्शक के रूप में प्रकट होते हैं। वह गुरु है। वह समग्र मानव जाति का होता है। वह आपके अन्तर्तम प्रकोष्ठ को खटखटाता तथा आपसे सानुकम्पा अनुरोध करता है : "हे भाग्यशाली मित्र! आप अज्ञान की गहन निद्रा से कब जागेंगे?... आइए! आइए! अब जग जाइए। इस स्वप्न को भंग कीजिए। अपने जन्मसिद्ध अधिकार की माँग कीजिए तथा अपने सत्स्वरूप को पहचानिए। अभी तथा यहीं पर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कीजिए तथा दिव्य आनन्द, शान्ति तथा ज्ञान के अनुभव में प्रवेश कीजिए जो कि आपका शाश्वत स्वरूप है।"
यह मानव-जाति को चिदानन्द का दिव्य आह्वान है। ईश्वर करे कि हम इस रोमांचकारी उद्बोधन पर ध्यान दें तथा गीता के अर्जुन की भाँति कहें: "करिष्ये वचनं तव" मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।
ॐ तत्सत्!
परिशिष्ट
(१)
माँ सरोजिनी के प्रति :
मातेश्वरी तू धन्य है!
माँ सरोजिनी तू धन्य है! मातृ-श्री तू धन्य है!
माँ सरोजिनी तू धन्य है! मातेश्वरी तू धन्य है!
श्रीधर-सरीखे सुत को, जन्म दिया तुम्हीं ने;
शिशु-क्रीड़ा, बाल-केलि का आनन्द लिया तुम्हीं ने।
तेरी कोख धन्य है, तेरी गोद धन्य है।
ममतामयी तू धन्य है, मातेश्वरी तू धन्य है।
ईश-प्रेम का संगीत सुनाया तुम्हीं ने,
मानव-सेवा का गीत सिखाया तुम्हीं ने।
तेरी ममता धन्य है, तेरी वत्सलता धन्य है।
नेहमयी तू धन्य है, मातेश्वरी तू धन्य है।।
दिव्य जीवन का बीज बोया तुम्हीं ने,
सन्त-जीवन का पाठ पढ़ाया तुम्हीं ने।
तेरा त्याग धन्य है, तेरा भाग्य धन्य है।
करुणामयी तू धन्य है, मातेश्वरी तू धन्य है।।
तेरा लाड़ला बना, शिवानन्द-दुलारा,
तेरे नयनों का तारा, जगत् का सहारा।
तुम्हारी शिक्षा धन्य है, तुम्हारी दीक्षा धन्य है।
जगज्जननी तू धन्य है, मातेश्वरी तू धन्य है।
'चिदानन्द' तुम्हारा प्राणधन है हमारा।
हृदय-धन तुम्हारा, जीवन-धन है हमारा।
तुम्हारा धाम धन्य है, तुम्हारा परिवार धन्य है।।
प्रातःस्मरणीया तू धन्य है, मातेश्वरी तू धन्य है।।
कोटि-कोटि प्रणाम माँ! तव श्री-चरणों में,
यही माँगते आज माँ कर-बद्ध तुम्हीं से।
सूरज-चन्दा जब लौं चमकै,
चिदानन्द-चन्द्र-वदन तब लौं दमकै।
दिव्य जीवन संघ धन्य है, शिवानन्द आश्रम धन्य है।
विश्व-वन्द्या तू धन्य है, मातेश्वरी तू धन्य है।
जब लौं गंग-जमुन की धारा, तब लौं जीये 'लाल' तुम्हारा।
पा कर तुम्हारे लाल को, अखिल विश्व धन्य है।
'शिवानन्द-दरबार' धन्य है, 'शिवानन्द-श्रीधाम' धन्य है।
परम आराध्या तू धन्य है, परम वन्दनीया तू धन्य है।
-श्रीधाम-परिवार
(२)
शिवानन्द स्वस्वरूप चिदानन्द है!
शिवानन्द स्वस्वरूप, आत्मरूप चिदानन्द हे।
शिवानन्द अभिन्नरूप, प्रतिरूप चिदानन्द हे।
शिवानन्द हृदयरूप, चित्तस्वरूप चिदानन्द है।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द हे ।।
गुरु भगवान्, गुरु गुणगान, गुरु ही प्राण मानी हे।
गुरु ही ज्ञान, गुरु ही ध्यान, गुरु ही प्रेम मानी हे।
गुरु ही दाता, गुरु ही माता, गोविन्दरूप निहारी है।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द हे।
प्रफुल्ल मुखमण्डल, स्वरूप मनोहारी हे।
सरस नैन, मंगल बैन, सर्वचित्त हारी हे।
ललित गान, मधुर तान, कोकिल कण्ठ पै वारी है।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द है।
अधर शुचि, हास उज्ज्वल, रूपहली दन्तावली है।
दीप्त भाल, कम्बु कण्ठ, गति गयन्दवारी है।
सर्वांग लसित, संग सुखद, प्रियदर्शी रूप निहारी है।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द है।
आजानु भुज, वरदहस्त, सर्व हितकारी है।
पादाम्बुज तरणिरूप, भव-वारिधि तारी है।
चापल्य मधुर, अति गम्भीर, पुण्यश्लोक जानी है।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द है।
भक्त-वृन्द-वन्दिते, त्रिविध तापहारी है।
अनाथ नाथ, करुणैक मूर्ति, सर्व सुखकारी हे।
विश्व-मण्डन, पाप-खण्डन, सर्व दुःखहारी है।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द है।
'तृणादपि सुनीचेन' विनीत रूप निहारी हे।
'अमानिना मानदेन' समदर्शी रूप निखारी हे।
'तरोरपि सहिष्णुना', शान्तचित्त विहारी है।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द हे ।।
महादानी, आत्मध्यानी, देहाध्यास न जानी है।
परम त्यागी, सदाचारी, पुण्य श्लोक मानी हे।
परोपकारी, रोगोपचारी, निज सुख-त्यागी हे।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द हे ।।
सर्वशास्त्र ज्ञान ज्ञाता, ज्ञानयोगी जानी हे।
ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, वीतरागी मानी है।
प्राण प्रणव, राजयोगी, कर्मयोगी मानी हे।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द है।
धर्म-प्रचारक, प्रेम-संचारक, जन-सेवा धर्म मानी हे।
कर्म-रत, मृदुल गात, वर्ण-भेद न मानी है।
परम भक्ति, परम शक्ति, सत्य अहिंसा मानी है।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द हे ।।
शिवानन्द-सन्देश सुरभि, दिव्योपदेश प्रसारी है।
सहज भाव रस-सिन्धु, काषाय वस्त्र धारी है।
या छवि पै बलिहारी हे, 'चेरी' सर्वस्व वारी है।
शिवानन्द आनन्दरूप, नमामि चिदानन्द हे ।।
-श्रीधाम-परिवार
(३)
गुरुदेव के प्रति
हे हृदयाराध्य देव!
चिदानन्द-चारु-चरित-भाषान्तर का दिया सुअवसर ।
किया धन्य-धन्य।
सामर्थ्य-हीन, शक्तिहीन, हैं साधन-हीन,
फिर भी हो हमें अपनाये :.
स्वतः ही तुम सदा हो हमारे।
अपने 'लाल' चिदानन्द का, करवाया
चरित प्रकाशित तुम्हीं ने
है यह अर्पण तुम्हें, करो स्वीकार
करो हमें कृतार्थ।
हे करुणामय गुरुदेव!
चिदानन्द-चरितामृत का जो करें पान
उनके लिए है यह दिव्यौषध एक,
बने संजीवनी समस्त रोगों की,
मिले सबको अभय दान।
-श्रीधाम-परिवार
विश्व-प्रार्थना
हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव!
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है।
तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ हो।
तुम सच्चिदानन्दघन हो।
तुम सबके अन्तर्वासी हो।
हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समत्व प्रदान करो।
हमें आध्यात्मिक अन्तःशक्ति का वर दो,
श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो।
जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों।
हम अहंकार, काम, लोभ, घृणा, क्रोध और द्वेष से रहित हों।
हमारा हृदय दिव्य गुणों से परिपूरित करो।
हम सब नाम-रूपों में तुम्हारा दर्शन करें।
तुम्हारी अर्चना के ही रूप में इन नाम-रूपों की सेवा करें।
सदा तुम्हारा ही स्मरण करें।
सदा तुम्हारी ही महिमा का गान करें।
तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे अधर-पुट पर हो।
सदा हम तुममें ही निवास करें।
-स्वामी शिवानन्द
इस पुस्तक के विषय में :
जीवन-स्रोत
इस पुस्तक में 'समत्व-योग' के मूर्तरूप परम पूज्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज के आकर्षक तथा अमिट प्रभावकारी आदर्श जीवन का चित्रण है। उनका जीवन सेवा, कर्म, भक्ति, जप, ध्यान, ज्ञान एवं राजयोग की सप्त धाराओं की सुन्दर मिलन-भूमि है तथा बिना किसी अपवाद के सभी जाति, वर्ण तथा धर्म के लोगों को प्रबोधन तथा पथप्रदर्शन प्रदान करता है।
आशा है, अध्यात्म के सभी पथिक, साधक, जिज्ञासु, भारतीय संस्कृति के प्रेमी तथा मानव-प्रेमी इस पुस्तक से प्रचुर प्रेरणा तथा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।