
श्रीमद्भगवद्गीता
मूल संस्कृत पाठ, शब्दार्थ, अनुवाद और व्याख्या
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती
अनुवादिका
श्रीमती गुलशन सचदेव
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण : २००५
द्वितीय हिन्दी संस्करण : २०१६
(१००० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
ISBN 81-7052-175-0
HS 25
PRICE: 425/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए
स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त
फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर, जि. टिहरी-गढ़वाल,
उत्तराखण्ड, पिन २४९१९२' में मुद्रित ।
For online orders and Catalogue visit: disbooks.org
|
समर्पित भगवान् व्यास एवं भगवान् कृष्ण को भगवान् विष्णु के अवतार वृन्दावन के मुरलीमनोहर देवकीनन्दन राधावल्लभ पतितोद्धारक अर्जुन के मित्र भक्तों के आदर्श
|
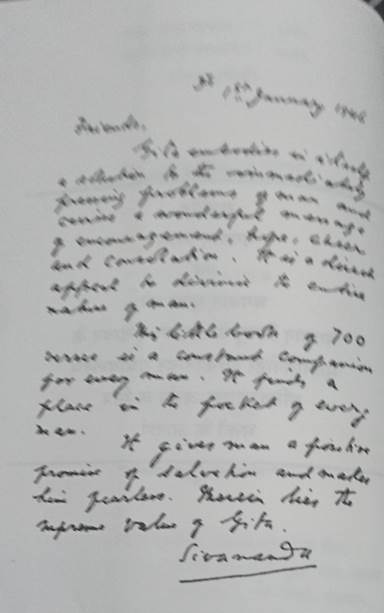
आमुख
भगवान् कृष्ण और अर्जुन के मध्य शुभ संवाद अथवा उपदिष्ट जीवन की परिभाषा ही भगवद्गीता है। इस अपूर्व ग्रन्थ का अनुवाद लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। विश्व-भर के दार्शनिक (तत्त्ववेत्ता), सन्तगण और अध्यात्मवादी इस ग्रन्थ से आकृष्ट हुए हैं। मानवता पर सम्भावित सभी कालों की समस्याओं का समाधान इसमें निहित है, यही भगवद्गीता की महिमा है। परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज दर्शन, धर्म और भगवद्गीता पद्धति के महान् अर्थप्रदर्शक हैं। सर्वाधिक आधिकारिक उपलब्ध टीकाओं में ही उनकी टीका को प्रशस्य स्थान प्राप्त है।
द डिवाइन लाइफ सोसायटी के प्रारम्भिक काल में यह ग्रन्थ छह भागों की श्रृंखला में प्रकाशित हुआ जिसके समस्त खण्ड पृथक् पृथक् थे। योग-साधकों का हितचिन्तन करते हुए पश्चात् काल में इस ग्रन्थ को एक समग्र, बृहत् स्वरूप दिया गया। अनेक संस्करण मुद्रित होने के पश्चात् कुछ काल के लिए यह ग्रन्थ अनुपलब्ध रहा। साधकों के कल्याण हेतु इसे पुनः प्रकाशित किया गया है। इसे यथासम्भव शुद्ध स्वरूप देने का हमारा पूर्ण प्रयास रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि साधक और सामान्य पाठकवृन्द इससे प्रशस्य रूप में लाभान्वित होंगे।
जुलाई १२, १९९५ -द डिवाइन लाइफ सोसायटी
विश्व-प्रार्थना
हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव!
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है।
तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ हो ।
तुम सच्चिदानन्दघन हो । तुम सबके अन्तर्वासी हो ।
हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समत्व प्रदान करो।
श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो ।
हमें आध्यात्मिक अन्तःशक्ति का वर दो,
जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों ।
हम अहंकार, काम, लोभ, घृणा, क्रोध और द्वेष से रहित हों।
हमारा हृदय दिव्य गुणों से परिपूरित करो ।
हम सब नाम-रूपों में तुम्हारा दर्शन करें।
तुम्हारी अर्चना के ही रूप में इन नाम-रूपों की सेवा करें।
सदा तुम्हारा ही स्मरण करें।
सदा तुम्हारी ही महिमा का गान करें।
तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे अधर-पुट पर हो ।
सदा हम तुममें ही निवास करें।
-स्वामी शिवानन्द
प्रार्थनाएँ
व्यास-वन्दना
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ।
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ।।
हे व्यास! भगवन्! आपको प्रणाम ! आपकी बुद्धि विशाल है। आपके नेत्र पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों के समान बृहत् हैं। आपने महाभारत रूपी तेल से पूर्ण ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया।
गुरु-वन्दना
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ।।
गुरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, गुरु पालनकर्ता विष्णु है, गुरु संहारकर्ता महेश्वर है। निश्चित रूप से गुरु साक्षात् ब्रह्मस्वरूप है। गुरु को प्रणाम ।
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ।।
गुरु की मूर्ति ध्यान का मूल है, गुरु के चरण पूजार्ह हैं, गुरु की वाणी मन्त्र रूप है और गुरु की कृपा मोक्षप्रदा है।
कृष्ण-वन्दना
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च।
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ।।
गो-रक्षक, नन्द गोप के प्रिय, देवकी को आह्लादित करने वाले वसुदेव-पुत्र श्री कृष्ण को पुनः-पुनः साष्टाङ्ग प्रणाम !
हे कृष्ण ! अब तुम मेरे प्रिय सखा हो। आपके हृदय में मेरे लिए दया का भाव है। अब मुझे अपनी दिव्य लीलाओं और वेदान्त के रहस्यों का बोध कराओ। आपने गीता में कहा है- "मैं वेदान्तकृत् और वेदवित् हूँ।" आप मेरे सर्वोच्च गुरु हो। वेदान्त की दुर्बोध समस्याओं को मेरे लिए स्पष्ट करो। मुझे सरल पाठ पढ़ाओ । कृपया बताओ-सर्वोच्च अद्वैत स्थिति, अद्वैत समाधि में स्थित, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी शुकदेव ने परीक्षित को 'भागवत' का उपदेश क्यों दिया? सायुज्य अवस्था का आनन्द लेने वाले भक्त, असम्प्रज्ञात समाधि में स्थित योगी और अद्वैत-अवस्थारूप-समाधि में लीन ज्ञानी के अनुभवों में क्या अन्तर है? जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति, तुरीया और तुरीयातीत, क्षरपुरुष और अक्षरपुरुष एवं पुरुषोत्तम-इनमें क्या अन्तर है?
हे कृष्ण, आप मेरे हृदय में निवास करते हो, मेरे मन के साक्षी हो और मेरे प्राणों के स्वामी हो; अतः मैं विमलात्मन् हो कर आपसे स्पष्ट बात करता हूँ। मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकता; क्योंकि मेरे मन से प्रभूत सभी विचारों के आप साक्षी हो । मुझे आपसे कोई भय नहीं। अब मेरे सखा हो आप । मेरे साथ अर्जुन की भाँति आचार करो। मैं गाऊँगा, नृत्य करूँगा। आप वंशी बजाओ । आओ! मिल कर माखन-मिश्री खायें। आओ! गीत गायें। मुझे गीता का ज्ञान दो। पुनः आपके मुखारविन्द से मुझे साक्षात् श्रवण करने दो।
हे दर्शनातीत प्रभो! मेरे आराध्य देव! इस विशाल ब्रह्माण्ड में अनन्त आकाश से ले कर मेरे पग तले की क्षुद्र घास पर्यन्त आपकी व्याप्ति और सूक्ष्म प्रवेशन है। इन सब नाम-रूपों के आप आधार हैं। आप मेरी आँख के तारे औ हृदय के दिव्य प्रेम हैं। आप मेरे प्राणों के प्राण, मेरे आत्मा के आत्मा, इन्द्रिय और बुद्धि के प्रकाशक, हृदय के मधुर संगीत-अनहत नाद और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों के सारतत्त्व हैं।
मैं तो केवल आपको ही इस सृष्टि के स्वामी और मेरे तीनों शरीरों के नियन्ता के रूप में जानता हूँ। भगवन् ! बारम्बार आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही मेरे केवल आधार हो। हे प्रेम और करुणा के सागर! आपके प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा है। उत्थान करो। उद्भासित करो। ज्ञानोद्दीप्त करो। पथ-प्रदर्शन करो। रक्षा करो। मेरे आध्यात्मिक पथ की बाधाओं को दूर करो। अज्ञान रूपी अविद्या का आवरण हटा दो। हे जगद्गुरु ! इस संसार के, इस जीवन के और इस शरीर के कष्ट अब और अधिक सहन नहीं होते, क्षण-भर को भी नहीं ! मुझे शीघ्र मिलो, प्रभो! मैं आपसे मिलने को लालायित हो रहा हूँ, द्रवित हो रहा हूँ, सुनो भगवन् सुनो, मेरी उत्कट आन्तरिक पुकार को सुनो। अत्याचारी मत बनो प्रभो! दीनबन्धु हो आप तो ! अधम-उद्धारक हो! पतित पावन हो !
हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव ! हे ज्ञान और आनन्द के मूल स्रोत! आप हमारे नेत्र के नेत्र हो, श्रोत्र के श्रोत्र हो, प्राण के प्राण हो, मन के मन हो, आत्मा के आत्मा हो। आप दृग्गोचर द्रष्टश हो, अश्रुत श्रोता हो, अचिन्त्य चिन्तक हो और अविदित वेत्ता हो । आपसे प्रार्थना है-हमें सब आसक्तियों से मुक्त कर दो, हमें ज्ञान दो, पवित्रता दो, प्रकाश दो।
प्रिय प्रभो! प्राणनाथ! विभु विश्वनाथ ! हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। हमारा मार्ग प्रशस्त करो। इस संसार के दलदल से हमें उबारो। हमें तेजस्वी बनाओ। हमारी रक्षा करो। हम केवल आपकी ही आराधना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका ही ध्यान करते हैं और आपके ही शरणागत हैं।
प्रस्तावना
गीता की महिमा
श्रीमद्भगवद्गीता भगवान् कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद रूप में महाभारत के भीष्म पर्व में निरूपित है। इस ग्रन्थ में अठारह अध्याय और सात सौ संस्कृत श्लोक समाविष्ट हैं। इन श्लोकों में महत्त्वपूर्ण (विचार्य) विषय संक्षेप में संवृत किया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन के साथ अत्यन्त मनोहारी, उपदेशात्मक संलाप में निगूढ़, उत्कृष्ट, आत्मोद्धारक आध्यात्मिक सत्यों को अनावृत किया और अर्जुन को योग, वेदान्त, भक्ति और कर्म के विरल रहस्यों का ज्ञान दिया। भगवान् कृष्ण के सभी उपदेश विस्तरशः मानव-कल्याण हेतु पश्चात्काल में भगवद्गीता के रूप में भगवान् वेदव्यास द्वारा लिपिबद्ध किये गये। जीवन में दैनिक आचार-व्यवहार, आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा आत्म-साक्षात्कार हेतु मानवता, श्री व्यास जी की अत्यन्त ऋणी है जिन्होंने इस दिव्य गीत को उनके समक्ष प्रस्तुत किया । श्रद्धायुक्त संयत मनुष्य ही 'गीता' का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं जो कि आत्मा का विज्ञान है।
हिन्दू पंचाङ्ग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को समस्त भारत में इस अद्भुत ग्रन्थ के प्रशंसकों और प्रेमियों द्वारा गीता-जयन्ती मनायी जाती है। इसी दिन संसार के समक्ष सञ्जय ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित किया ।
विश्व के साहित्य में गीता के समान प्रेरक एवं उत्कृष्ट ग्रन्थ अन्य नहीं है। हिन्दू धर्म के सारभूत प्रधान नियम अत्यन्त स्पष्ट रूप से गीता में वर्णित हैं। यह प्रज्ञा का स्रोत है। आपका पथ-प्रदर्शक है। परम गुरु है। अक्षय आध्यात्मिक कोष है। आनन्द का निर्झर है। ज्ञान का रत्नाकर है। यह ग्रन्थ दिव्य कान्ति और विभूति से परिपूर्ण है।
गीता वेदों का सार है। उपनिषदों का निष्कर्ष है। सभी कालों में सभी प्रकार के लोगों के लिए यह एक सार्वभौम शास्त्र है। उन्नत विचारों और योग, भक्ति, वेदान्त तथा कर्म के व्यावहारिक आदेशों से युक्त यह अद्वितीय ग्रन्थ है। निगूढ़ विचारों और अन्तर्दृष्टि के सर्वोच्च शिखर का स्पर्शबोध है यह अद्भुत ग्रन्थ। इस संसार के त्रिविध तापों से क्लिष्ट आत्माओं को यह ग्रन्थ शान्ति और समाश्वासन प्रदान करता है अर्थात् आध्यात्मिक (शरीर से उत्पन्न होने वाली पीड़ा), आधिभौतिक (प्राणियों से उत्पन्न) एवं आधिदैविक (देवकृत्) पीड़ा ।
भगवद्गीता दिव्य सुधा है। यह चिन्तामणि (चिन्तन मात्र से कामनापूर्ति करने वाली मणि) है, कल्पतरु और कामधेनु है जो कल्पना मात्र से इच्छापूर्ति करती है। आप इसमें से मनोवांछित वस्तु ले सकते हैं। यह आनन्त्य शास्त्र है। यह मशरूम की भाँति अल्पकालिक नहीं है। मैं गीता को सदा अपने पास रखता हूँ। यह सबके लिए सहचरी (vade mecum) पुस्तिका है। शान्ति, आनन्द, सुख, प्रज्ञा, आत्मा, ब्रह्म, पुरुष, धाम, निर्वाण, परम पद, गीता-ये सभी पर्यायवाची हैं।
गीता अमृत का महापयोधि है। यह उपनिषदोपम वृक्ष का दिव्य अमर फल है। इस अलौकिक ग्रन्थ में कर्म, भक्ति और ज्ञान दर्शन का तथा इनके संयोगात्मक विवरण का निष्पक्ष स्पष्टीकरण मिलता है। भगवद्गीता विश्व-भर में मंजुल सुगन्धि विकीर्ण करने वाला विरल और अतिशोभन पुष्प है। सभी उपनिषद् मानो गाय हैं, श्री कृष्ण उपनिषद् रूपी गायों के दोग्धा हैं, अर्जुन बछड़ा है जिसने आत्म-ज्ञान रूपी दुग्ध का सर्वप्रथम पान किया जो समस्त मानवता और अर्जुन के कल्याणार्थ दिव्य 'गोपाल' श्री कृष्ण द्वारा 'गीता' के रूप में दुहा गया। गीता द्वारा न केवल अर्जुन प्रत्युत् प्रत्येक व्यक्ति की शंकाओं और समस्याओं का समाधान होता है। देवकीनन्दन, गोकुल के गोप-मित्र भगवान् कृष्ण की जय हो! हृदय की पवित्रता और ध्यान द्वारा जो गीतामृत पान करता है वह अमृतत्व, शाश्वत आनन्द, चिर-शान्ति और अक्षय्य सुख का अनुभव करता है।
जिस प्रकार सघन अगाध सागर की गहराई अमूल्य रत्नों का भण्डार है उसी प्रकार गीता में अगणित आध्यात्मिक रत्न निहित हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको गीता रूपी रत्नाकर में गहन अवगाहन करना होगा। तभी तो आप आध्यात्मिक मुक्ता-मणियाँ चयन कर पायेंगे। गीता के सूक्ष्म गहन ज्ञान को भी तभी आप समझ पायेंगे।
सभी कालों के लिए गीता एक अनुपम शास्त्र है। हिन्दू धर्म के प्रामाणिक शास्त्र 'प्रस्थानत्रयी' की श्रेणी में गीता को माना जाता है। गीता, जीवन की महत्ता को दर्शाने वाला आत्मा का अमर गीत है। भगवान् कृष्ण द्वारा दिये गये गीता के उपदेश समस्त संसार के लिए अनुकरणीय हैं। यह योग का विशिष्ट ग्रन्थ है। इसकी भाषा अत्यन्त सरल है। संस्कृत भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इसका अध्ययन कर सकता है। इसमें चार प्रकार के योग निरूपित हैं-कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग और ज्ञानयोग ।
आज तक गीता पर असंख्य टीकायें उपलब्ध हैं। प्रत्येक श्लोक पर एक खण्ड लिखा जा सकता है। कर्म में आस्था रखने वाला व्यस्त व्यक्ति श्री बालगङ्गाधर तिलक की टीका (गीता-रहस्य) से लाभान्वित हो सकता है, भक्ति भाव से पूर्ण व्यक्ति श्रीधर की टीका पढ़े और तर्कशील व्यक्ति श्री शंकराचार्य की टीका से लाभ उठा सकता है।
इस अलौकिक ग्रन्थ पर सैकड़ों टीकायें उपलब्ध हैं। गीता एक सागर है। श्री शंकर, श्री रामानुज और श्री मध्वाचार्य ने गीता पर अपनी-अपनी व्याख्या की है और इस प्रकार दर्शन के अपने मत प्रतिपादित किये। कोई भी व्यक्ति गीता-सिन्धु में गहन अवगाहन कर के दिव्य ज्ञान रूपी अमूल्य मोती ला सकता है और व्याख्या रूप में प्रस्तुत कर सकता है। गीता का स्तवन हो ! गीता के भगवान् का स्तवन हो!
गीता के उपदेश उदार, सार्वभौमिक और उत्कृष्ट हैं। इसके उपदेश किसी विशेष जाति, मत, धर्म, आयु, स्थान अथवा देश के लिए नहीं प्रत्युत् समस्त विश्व के लिए हैं। उपनिषदों पर आधारित ये उपदेश ऋषियों के सनातन ज्ञान का कोष हैं। इसकी विधा (पद्धति) सबके लिए बोधगम्य है। मानव मात्र के लिए इसमें सान्त्वना, शान्ति, स्वाधीनता, मोक्ष और पूर्णत्व का सन्देश है।
परमहंसों (यति, संन्यासी) के लिए गीता मानसरोवर झील है और पिपासु साधकों के लिए क्रीड़ा का विषय है । यह आनन्द-पयोधि है जिसमें सत्यान्वेषक हर्षोल्लास और मस्ती में प्लवन (तरण) करते हैं। यदि स्पर्शमणि (पारस) किसी लोहे के टुकड़े को एक कोण से भी स्पर्श कर ले तो पूर्ण लौह-खण्ड स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाँति आप किसी एक श्लोक के भाव में भी मग्न रहेंगे, तो निस्सन्देह आप दिव्यत्व में रूपान्तरित हो जायेंगे।
दैनिक स्वाध्याय हेतु केवल गीता का अध्ययन ही पर्याप्त है। इसमें सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। जितना अधिक श्रद्धा और विश्वास से आप इसका अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक गूढ़ ज्ञान, सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि और स्पष्ट, यथार्थ चिन्तन आपका होगा। गीता के एक श्लोक के भाव में लीन रहने पर भी आपके समस्त दुःखों का अन्त होगा, आप जीवन के लक्ष्य-अमरत्व और शाश्वत शान्ति प्राप्त करेंगे।
गीता का संवाद सम्पूर्ण विश्व के लिए है। मनुष्य-जाति के प्रधान भाग के लिए है। कुरुक्षेत्र के मैदान में यह ज्ञान भगवान् कृष्ण द्वारा अर्जुन को आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व दिया गया था।
भगवान् के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसे अभूतपूर्व, अद्भुत ग्रन्थ को प्रकाश में नहीं ला सकता। पाठकों का पथ प्रशस्त करने वाला, परमानन्द की प्राप्ति में उन्नायक, सहायक और शान्तिप्रद यह ग्रन्थ आज भी जीवन्त है। ज्ञान-स्वरूप, मोक्षदायक परमात्मा के अस्तित्व का यह साक्षात् प्रमाण है।
सम्पूर्ण विश्व ही एक युद्धक्षेत्र है। वास्तविक कुरुक्षेत्र तो आपके भीतर है। महाभारत का युद्ध अभी भी आपके भीतर पूर्ण उग्रता से चल रहा है। अविद्या धृतराष्ट्र है। जीवात्मा अर्जुन है। हृदय-गुहा में विराजित भगवान् कृष्ण सारथि हैं। शरीर आपका रथ है। इन्द्रियाँ अश्व हैं। मन, अहंभाव, इन्द्रियाँ,
संस्कार, वासनायें, इच्छायें, राग-द्वेष, काम, ईर्ष्या, लोभ, अभिमान और दम्भ (कपट) आपके घोर शत्रु हैं।
अध्ययनार्थ प्रकाशदीप
गीता में सूक्ष्म गूढ़ ज्ञान निहित है, अतः आपको महती श्रद्धा, अनन्य भक्ति और अत्यन्त शुचिता से किसी पारंगत विद्वान् अथवा ब्रह्म-निष्ठ गुरु के सान्निध्य में इसका अध्ययन करना चाहिए। गीता के सत्यार्थ करतल पर रखे फल की भाँति तभी प्रकट होंगे। स्वामी मधुसूदन सरस्वती, स्वामी शंकरानन्द और श्री शंकराचार्य जैसे प्रबुद्ध ज्ञानियों की टीकायें आपके लिए अतीव उपयोगी रहेंगी।
सांसारिक लोग कितने ही बुद्धिमान् क्यों न हों, गीता के मूल उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते। वे अनावश्यक वाद-विवाद और निरर्थक तर्क में फँस जाते हैं। वे मिथ्यावाद और उपदेशों के छिद्रान्वेषण में लग जाते हैं। अज्ञानी पुरुष यही कहेंगे-“श्लोकों में अन्तरंग सम्बन्ध नहीं है। वे अव्यवस्थित रूप से संहत किये गये हैं। उनमें पुनरावृत्ति है।" यदि वे किसी विद्वान् से श्रद्धा और विश्वास के साथ गीता का अध्ययन करें, तो उनके समस्त सन्देह नष्ट हो जायेंगे। उन्हें यह ज्ञान भी हो जायेगा कि सभी अध्यायों में सभी श्लोकों का अन्योन्य निकट सम्बन्ध है। उपनिषदों में और गीता में पुनरावृत्ति उपयुक्त है। मन पर गम्भीर स्थायी प्रभाव डालने के लिए ऐसा किया जाता है।
भगवान् कृष्ण चेतना के विभिन्न स्तरों से वचन कहते हैं। गीता में 'अव्यक्त' शब्द कहीं तो मूल प्रकृति के भाव में आया है और कहीं-कहीं परब्रह्म के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। अतः श्लोकों का वास्तविक अर्थ जानने के लिए मनीषी शिक्षक की सहायता आवश्यक है। कठोपनिषद् में 'इष्टकाः' शब्द का अर्थ देवता है। हठ योग में कहा है- “गङ्गा और यमुना के संगम पर एक युवती कन्या है।" इसका विशिष्ट अर्थ है- “इड़ा और पिंगला के मध्य सुषुम्ना नाड़ी है।" गुरु के बिना ऐसे शब्दों का अर्थ समझना कठिन है। इसी प्रकार से गुरु के बिना गीता के श्लोकों का अर्थ-बोध दुर्गम है। अन्यथा आप उस व्यक्ति के समान ही रहेंगे जो भोजन करने वाले व्यक्ति द्वारा 'सैन्धव' माँगने पर घोड़ा ले आया; क्योंकि सैन्धव शब्द का अर्थ घोड़ा भी है और नमक भी।
गीता में समन्वय
मनुष्य तीन मूल घटकों का योग है-संज्ञान, भाव और इच्छा। मानव-प्रकृति त्रिविध है-क्रियाशील, भावुक और ज्ञानशक्ति सम्पन्न । अतः तीन प्रकार के योग आचक्षित हैं-ज्ञानयोग जो आत्म-विश्लेषण करने वाले चिन्तनशील प्रकृति के मनुष्य के लिए है। भक्तियोग भावुक लोगों के लिए और कर्मयोग क्रियाशील (राजसिक) व्यक्तियों के लिए है। एक योग अन्य योग की भाँति ही प्रभावपूर्ण है।
गीता में तीन मार्गों के सिद्धान्त के निर्देशन हैं, वे हैं-ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग । गीता के उपदेशों के अनुसार तीनों में कोई विरोध नहीं है। कर्म, भक्ति और ज्ञान दर्शन को गीता अद्भुत रूप से सूत्रबद्ध करती है। पूर्णत्व की प्राप्ति हेतु तीनों में अनुरूपता लाना अत्यन्त आवश्यक है। तदर्थ आपके पास श्री शंकर का मस्तिष्क, भगवान् बुद्ध का हृदय और राजा जनक का हस्त होना आवश्यक है। इस शरीर रूपी रथ के तीन घोड़े-कर्म, भाव और बुद्धि में सामञ्जस्य हो, तभी यह रथ सहज रूप से चलेगा और आप अपने लक्ष्य तक अचिरेण सुरक्षित पहुँच सकते हैं। अपनी अन्तरात्मा में तभी आप आनन्दित हो सकते हैं। केवल तभी आप 'सोऽहम्' का गीत गा सकते हैं। केवल तभी आप 'अनन्त' के साथ समस्वर हो सकते हैं। केवल तभी आप आत्मा का अनहत नाद श्रवण कर सकते हैं और आत्मा के मधुर सङ्गीत का रसपान कर सकते हैं। स्वधर्म का पालन करते हुए पूर्णत्व, मोक्ष अथवा चरम लक्ष्य की प्राप्ति ही गीता का प्रमुख उपदेश है। भगवान् कृष्ण अर्जुन से कहते हैं-अतः अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करो; क्योंकि आसक्ति रहित हो कर कर्म करने से मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त होता है।
सामवेद के महावाक्य 'तत्-त्वम्-असि' (तत्त्वमसि) अर्थात् 'वह तुम हो' की व्याख्या के आधार पर गीता तीन भागों में विभक्त है। इस विचारधारा के अनुसार प्रथम छह अध्याय कर्मयोग और 'त्वम्' पद की प्रकृति का निरूपण करते हैं। इसके पश्चात् के छह अध्याय भक्तियोग और 'तत्' पद का दर्शन कराते हैं। अन्तिम छह अध्याय ज्ञानयोग और 'असि' पद का ज्ञान कराते हैं जो 'जीव-ब्रह्म-ऐक्य' संस्थापन करने में समर्थ है।
गीता के अठारह अध्याय असमन्वित रूप से सूत्रबद्ध नहीं हैं। एक अध्याय का दूसरे के साथ निकट का सम्बन्ध है। अर्जुन की विषादपूर्ण अवस्था में दूसरे अध्याय के उपदेशों से उसके नेत्र खुले और आत्मा की नित्यता को प्रदीप्त करने वाले वचनों से उसे पुनः शक्ति और साहस मिला। तब अर्जुन ने कर्मयोग और कर्मफल-त्याग का अवबोध किया। उसने इन्द्रियों और मन का संयम तथा एकाग्रता और ध्यान की विधियों को सीखा । तदुपरान्त भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को विश्व-रूप-दर्शनार्थ तैयार करने के लिए उसके समक्ष विविध विभूतियों का विवरण दिया। अर्जुन ने अतिशोभन (देदीप्यमान) विश्व दर्शन का अनुभव किया। तब उसने जीवन्मुक्त की प्रकृति को समझा। उसे क्षेत्र ज्ञान, तीन गुणों के ज्ञाता और पुरुषोत्तम का ज्ञान हुआ। इसके पश्चात् अर्जुन ने दिव्य विभूतियों, तीन प्रकार की श्रद्धा और अन्त में संन्यासयोग के सार का ज्ञान ग्रहण किया। जिस प्रकार किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में ज्ञान दिया जाता है, उसी प्रकार भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आत्म-ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन की विभिन्न शंकायें थीं। भगवान् कृष्ण ने उसकी सभी शंकाओं का एक-एक करके निवारण किया। योग के एक सोपान से दूसरे सोपान तक आरोहण हेतु उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया। अन्ततः अर्जुन ने सर्वोच्च सोपान पर अपना पग रखा, आत्म-ज्ञान प्राप्त किया और हर्षित हो कर बोला-"हे मेरे प्रभो! मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हो गया है। अब मैं कृतसंकल्प हूँ। मेरे सन्देह पूर्णतया नष्ट हो गये हैं। अब मैं आपके वचन का परिपालन करूँगा।"
राग-द्वेष और अहंभाव का विनाश करके आप जीवन्मुक्त हो सकते हैं। इच्छाओं, तृष्णाओं, अवशिष्ट संस्कारों और संकल्पों का विनाश करके आप मुक्त संन्यासी हो सकते हैं। एवंविध, निज सच्चिदानन्द स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हुए आप राजा जनक की भाँति संसार के क्रिया-कलापों में रत भी रह सकते हैं। आप तब कर्म-बन्धन में नहीं पड़ेंगे और कर्म आपको दूषित नहीं करेंगे; क्योंकि ब्रह्मज्ञान से कर्तापन का भाव नष्ट हो चुका है। यही गीता का सार है।
दो विधाएँ
उपनिषदों के ऋषि गौरव से घोषणा करते हैं कि वास्तविक पुरुष सर्वव्याप्त, अमर आत्मा है जो इस शरीर, मन और जगत् का आधार है और पाँच कोषों-अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोष का भी आश्रय है।
दुग्ध में नवनीत और काष्ठ में अग्नि की भाँति इस शरीर में निहित स्वयंज्योतित आत्मा का साक्षात्कार ही इस जीवन का लक्ष्य है। आत्मा अन्तर्यामी है। शरीर रूपी भवन का वह अदृश्य शासक अथवा गुप्त स्वामी है।
सतत गहन ध्यान द्वारा उस अक्षय्य, अमर्त्य, भावातीत आत्म तत्त्व की प्राप्ति ही सत्य धर्म है। शाश्वत आत्मा में जीवन ही वास्तविक जीवन है। भूत, भविष्य और वर्तमान से अतीत, आदि, अन्त और मध्य से परे उस आत्म तत्त्व के न तो खण्ड हैं और न ही अवयव, न वह स्थूल है, न सूक्ष्म, ऐसे परम तत्त्व के साथ ऐक्य भाव पूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन है।
पुरातन ऋषियों ने इस रहस्यमय अलौकिक आत्म तत्त्व को दिव्य ज्ञानचक्षुओं से आत्मसात् किया और उसी आत्म-ज्ञान की ज्योति से संसार के पदार्थों को उजागर किया। यह आत्म-बोध की साक्षात् प्रमाण की विधि है।
संगीत, प्रकृति, कला और विज्ञान के द्वारा आप ज्ञान-गिरि-शिखर तक आरोहण कर सकते हैं। यह अप्रत्यक्ष विधि है। आप कार्य से कारण तथा अन्ततः कारण रहित कारण परब्रह्म इन्द्रियातीत सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पाश्चात्य वैज्ञानिकों का प्रयोजन यदि मनुष्य को भौतिक सुख प्रदान करना ही है तो वे मानो अन्धकार में कुछ टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान का लक्ष्य अन्वेषण, परीक्षण, निरूपण, विश्लेषण और अध्ययन द्वारा प्रकृति के नियमों तथा अणु, परमाणु ऊर्जा, गति तथा शारीरिक और मानसिक प्रपंच (दृश्य जगत्) के आत्यन्तिक सत्य का आधार खोजना है। सच्चा वैज्ञानिक तो केवल वेदान्ती है। सत्य के प्रति उसकी खोज की विधा पृथक् है। जो वैज्ञानिक पहले यह कहते थे-"इस संसार से परे कुछ नहीं है", आज वही घोषणा करते हैं- "जितना अधिक मैं इस दृश्य जगत् का ज्ञान करता हूँ, उतना अधिक मैं भ्रमित होता हूँ। बुद्धि प्रमेय और भावशून्य है। इस परिवर्तनशील प्रपंच से परे कूटस्थ बोधगम्य शक्ति है। चक्रावर्तिन् जीवन्त विद्युत् कणों के पीछे स्थिर, गतिशून्य शक्ति है जो बुद्धि और जगत् से अतीत है।" उपनिषदों का ब्रह्म वेदान्त का आत्मा है जो प्रकृति के नियमों का अधिष्ठाता है। “समुपगमन (approach) की मेरी विधा उत्तरकालीन है अर्थात् कार्य से कारण की ओर। वेदान्ती विधा पूर्वकालीन है अर्थात् कारण से कार्य की ओर उपगमन । दोनों का लक्ष्य एक है।"
दो मार्गों का सन्धान
विष्णु पुराण में भगवान् विष्णु की उत्कृष्ट रूप से गुणस्तुति की गयी है और भगवान् शिव को गौण स्थान दिया गया है। शिव पुराण में भगवान् शिव का स्तवन मुख्य है और भगवान् हरि का गौण । देवी भागवतम् में देवी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और भगवान् शिव तथा भगवान् हरि को गौण । साधक के हृदय में अपने इष्टदेव के प्रति प्रगाढ़, अटूट श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। शिव, हरि और देवी एक ही हैं। वे तो भगवान् के विभिन्न स्वरूप हैं। शिव को हरि से और हरि को शिव से गौण समझना मूर्खता है।
एवंविध, एक स्थान पर भगवान् कृष्ण कर्मयोग की श्लाघा करते हैं-"कर्म संन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते"-"निश्चित रूप से कर्मयोग कर्म-संन्यास से श्रेष्ठतर है" (५/२) । अन्य स्थान पर वे योग को सर्वोच्च स्थान देते हुए कहते हैं-"योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, वह ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है; कर्मयोगी से भी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन ! तू योगी बन जा" (६/४६) । एक अन्य स्थान पर भगवान् भक्तियोग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं- "वह परम पुरुष तो हे पार्थ, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्य है" (L / R * R) । एक अन्य स्थान पर वे ज्ञानयोग की स्तुति में कहते हैं- "यह सभी उदार हैं; किन्तु ज्ञानी तो मेरा आत्म-स्वरूप है, आत्मवत् वह मुझमें स्थित है जो कि अन्तिम लक्ष्य है" (७/२२)।
अनभ्यस्त नव-साधक इन श्लोकों को पढ़ कर भ्रमित हो जायेगा; किन्तु गहन चिन्तन किया जाये, तो भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं रहता। साधक के हृदय में निज मार्ग-विशेष के प्रति आस्था जागृत करने के लिए भगवान् कृष्ण ने प्रत्येक योग की प्रशंसा की है। स्मरण रहे, गीता समस्त विश्व के लिए पठनीय ग्रन्थ है। यह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं सुनायी गयी। प्रत्येक योग समान रूप से प्रभावपूर्ण और प्रबल है।
गीता का सार
गीता पुनः-पुनः साधक को अनासक्त वृत्ति अंकुरित करने का प्रबल उपदेश देती है। बारम्बार गीता का यही सन्देश मिलता है कि संसार में ऐसे रहना चाहिए जैसे जल में कमल-पत्र-जल से सर्वथा अप्रभावित। जो मनुष्य अनासक्त भाव से सभी कर्म प्रभु को समर्पित करके करता है, वह जल में कमल-पत्र की भाँति पाप से अप्रभावित रहता है, "पद्मपत्रमिवाम्भसा" (५/२२) ।
मोह आसक्ति का कारण है। आसक्ति रजस् गुण का प्रतिफल है। अनासक्ति सत्त्व से उत्पन्न होती है। आसक्ति आसुरी सम्पदा है। अनासक्ति दैवी सम्पदा है। आसक्ति अज्ञान, स्वार्थ और मोह से होती है। आसक्ति मृत्यु का कारण है। अनासक्ति ज्ञान है। अनासक्ति से मोक्ष-प्राप्ति होती है। वस्तुतः अनासक्ति का अभ्यास कठोर अनुशासन है। इसका अभ्यास पुनः-पुनः करना होगा। सम्भव है चलना सीखते हुए शिशु की भाँति आप गिर पड़े; किन्तु प्रफुल्ल हृदय से, मुस्कराते हुए आपको पुनः उठना पड़ेगा। असफलतायें अवरोध नहीं हैं, वे तो सोपान हैं सफलता के। आत्मस्थ होने का प्रयास करो । अपनी ही आत्मा में स्थित रहो। अपनी परिधि में रहो। सतत आत्म-चिन्तन करो। स्वभावतः ही सभी आसक्तियाँ नष्ट हो जायेंगी। भौतिक आसक्तियों के विनाश हेतु आत्मा अथवा परमात्मा से आसक्ति प्रबल प्रतिकारक का कार्य करती है। अनासक्त व्यक्ति ही दूसरों से प्रेम कर सकता है। उसके पास दिव्य प्रेम है। अतः आसक्ति रहित हो कर निरन्तर कर्म में रत रहना कर्तव्य है; क्योंकि आसक्ति रहित हो कर कर्म करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है।
अध्याय तेरह, चौदह और पन्द्रह ज्ञानयोग को प्रतिपादित करते हैं। जिसे प्रकृति और पुरुष का ज्ञान है, तीन गुण और उनके व्यापार का ज्ञान है और माया रूपी अद्भुत संसार-वृक्ष का ज्ञान है, वह प्रकृति और उसके गुणों का अतिक्रमण कर के अनासक्ति और आत्म ज्ञान के खड्ग से इस अनोखे बद्धमूल (संसार) वृक्ष को काट कर जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त करने वाले आत्म-साक्षात्कार की सद्यः अनुभूति कर सकता है। अध्याय पन्द्रह आत्मा को प्रेरित करने वाला है। इसमें वेदान्त का सार निहित है। इस प्रवचन को अवधारण करने वाला व्यक्ति अचिरेण मोक्ष-प्राप्ति करता है। वह परब्रह्म के अनश्वर धाम को पहुँचता है। इन बीस श्लोकों को कण्ठस्थ करो और भोजन से पूर्व इनका उच्चारण करो। भोजन ग्रहण करने से पूर्व सभी संन्यासी इसका गान करते हैं।
अध्याय अठारह पुनः-पुनः पढ़ने योग्य है। सम्पूर्ण गीता शास्त्र का सार इसमें निहित है। गीता-ज्ञान रूपी अनुपम शैल-पाद का यह सर्वोच्च शिखर है। यह अमूल्य हार का मुकुट मणि है। इसी में प्रथम सत्रह अध्यायों के उपदेशों के सार संक्षेप में आचक्षित हैं।
दूसरे अध्याय के श्लोकों में १९,२०,२३ और २४ नम्बर के श्लोकों की अनवरत स्मृति और अभ्यास आप पर अमरत्व की वृष्टि करेंगे और भय तथा देहाध्यास (शरीर और आत्मा में ऐक्य भाव) का निवारण करेंगे।
'ये हि संस्पर्शजा भोगा...' (५ /२२) , 'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्..." (१३/ ८) और 'विषयेन्द्रिय संयोगात्...' (१८/३८) की शिक्षाओं का सतत अभ्यास और स्मृति वैराग्य लाने में सक्षम हैं।
अध्याय २ के श्लोक ७१ और अध्याय ४ के श्लोक ३९ परम शान्ति के देने वाले हैं। अध्याय ५ के श्लोक २७ और २८, अध्याय ६ के श्लोक ११ से १४ और २६, अध्याय ८ के श्लोक ८,१२,१३ और १४, अध्याय ९ को श्लोक ३४, अध्याय १२ के श्लोक ८ से १० और अध्याय १८ के श्लोक ५१ से ५३ आत्म-साक्षात्कार हेतु अध्यात्म-साधना-योग-साधना में पथ प्रदर्शित करते हैं। अध्याय २ श्लोक ११ से गीता-दर्शन प्रारम्भ होता है। अध्याय १८ का श्लोक ६६ गीता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है- "सब धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जाओ, शोक मत करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा।" भगवान् कृष्ण से अर्जुन कहते हैं- "मेरा हृदय लघुता से आहत है, मेरा मन किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ-निश्चित रूप से मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, वह बात कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए।" अध्याय २ के श्लोक ७ में अर्जुन द्वारा पूछे गये इस प्रश्न का उत्तर भगवान् कृष्ण अध्याय १८ के श्लोक ६६ में देते हैं। सम्पूर्ण गीता का सार अध्याय १८ के श्लोक ६५ और ६६ में अन्तर्निहित है।
अध्याय १८ के श्लोक ६५ में 'नवधा भक्ति' का सार निहित है। मनोवृत्तियों के दमन की साधना यही है। पुनः पुनः भगवान् पर मन एकाग्रित करने से सभी सांसारिक विचार नष्ट हो जाते हैं। भक्तियोग को कदाचित् ही राजयोग से पृथक् किया जा सकता है। ये दोनों योग एकरूप हैं। महर्षि पतञ्जलि कहते हैं कि भगवान् के प्रति भक्ति से ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है- 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' अर्थात् आत्म-समर्पण से। क्रियायोग और राजयोग के नियम में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 'मन्मना भव' का अभिप्राय है-मन को लीन करना। यह राजयोग साधना है। भक्तियोग कहाँ समाप्त होता है और राजयोग कहाँ प्रारम्भ होता है, यह कहना कठिन है। राजयोग भक्तियोग का पूरक है। भक्तियोग और राजयोग के मध्य कोई सीमारेखा अथवा दृढ़ नियम नहीं है। राजयोगी एक भक्त भी है और भक्त एक राजयोगी है। केवल नाम भिन्न हैं। भ्रमित और निराश अवस्था से ग्रस्त अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए भगवान् कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करने के लिए ये वचन कहते हैं- “तुम मुझे प्राप्त होओगे। मैं तुम्हें सत्य वचन कहता हूँ, तुम मुझे प्रिय हो।" अध्याय अठारह के श्लोक ६५ के इन उपदेशों का पालन करो। जिसने इन चार महान् उपदेशों का पालन कर लिया, वह असमय अप्रतिज्ञ समर्पण भाव लाने में सक्षम होगा।
अगला श्लोक आत्म-समर्पण का भाव दर्शाता है। अद्वैत वेदान्ती के अनुसार इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी- "व्यष्टिभाव को त्याग दो। तुम मोक्ष प्राप्त करोगे । तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे।" भक्तिपन्थ का आचार्य इस प्रकार व्याख्या करेगा - "सभी कर्म और कर्मफल भगवान् के चरणों में अर्पित कर दो। भगवान् तुम्हें मुक्त करेंगे।" यहाँ धर्म का अर्थ इन्द्रिय-धर्म से नहीं है; क्योंकि जीवन्मुक्त भी देखता है, सुनता है, स्वाद लेता है और इसी प्रकार अन्य कार्य करता है, किन्तु वह ये सब साक्षीभाव में (द्रष्टा बन कर) करता है। इन्द्रियों के कर्म में वह स्वयं को एकरूप नहीं कर लेता। अर्जुन की जिज्ञासा का नियत उत्तर भगवान् कृष्ण इस श्लोक में देते हैं।
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।।
और अर्जुन की जिज्ञासा थी- “मेरा हृदय लघुता से आहत है। मैं किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, निश्चित रूप से मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, उसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए।"
योग-वेदान्त पर अधिक पुस्तकों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। यदि उन दो श्लोकों के भाव में आप लीन रह सकते हैं तो अमृतत्व, शाश्वत आनन्द और आत्म-ज्ञान की प्राप्ति होगी।
“अहंभाव त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म और उसके फल भगवान् की सन्तति मान कर उन्हें समर्पित कर दो। मन और अहंता भगवान् को दे कर जीवन को दिव्य बनाओ। मन और बुद्धि उन्हें दे कर जीवन को आध्यात्मिक बना लो (मच्चित, युक्त, मत्परः) । भगवान् पर मन एकाग्र करो । उनके प्रति भक्तिभाव अर्जित करो। सब प्राणियों के कल्याण में लग जाओ (सर्वभूत हिते रतः) । सर्वस्व भगवान् को अर्पित कर दो, तभी उनकी सत्ता में प्रवेश पा सकोगे।" सम्पूर्ण गीता में यही स्वर झंकृत हो रहा है।
गीता में साधना निम्न श्लोकों में निरूपित है :
कर्मयोग-२/४८; ४/२०,२१, २२ और २४
भक्तियोग -९/२७,३४; १२/८; १८/५२,५३ और ५४
जपयोग-८/१४
अभ्यासयोग - १२/९
हठयोग-८/१० और १२
राजयोग-६/२५ और २६
ज्ञानयोग-३/२८; ५/८ और ९
रक्षण
गीता का अध्ययन, कुछ लोग उसमें निहित उपदेशों में छिद्रान्वेषण अथवा आलोचनात्मक दृष्टिकोण ले कर करते हैं। किन्तु प्रगाढ़ श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि अध्ययन किया जाये, तो गीता के उपदेश बोधगम्य हो सकते हैं।
एक व्यक्ति ने समाचार-पत्र में आलोचनात्मक आक्षेप इस प्रकार दिया- "गीता पावन ग्रन्थ कदापि नहीं है। यह तो हिंसा का पाठ पढ़ाती है। भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को अपने सम्बन्धियों और गुरुजनों की हिंसा के लिए आज्ञा दी ।'' ऐसा प्रतीत होता है, इस समालोचक को गीता का ज्ञान ही नहीं था। वह विरोचन की भाँति है जिसने प्रजापति से आध्यात्मिक शिक्षा तो ग्रहण की, परन्तु अपनी कुटिल मति के कारण शरीर को ही आत्मा मान लिया। निश्चित रूप से वह आमिष (दैहिक) दर्शन का अनुयायी होगा। वह गीता के दार्शनिक पक्ष की गम्भीरता को समझने में सक्षम नहीं है; क्योंकि उसकी बुद्धि स्थूल और दुर्भेद्य होने के कारण सत्य को ग्रहण नहीं कर सकती । आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु उसने गीता नहीं पढ़ी, प्रत्युत् आक्रामक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया है। यदि वास्तव में उसने इन निम्न तीन श्लोकों का महत्त्व जान लिया होता तो व्यर्थ की आलोचना न की होती । वे श्लोक हैं-
"जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मान लेता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं; क्योंकि न तो वह मारता है और न ही मरता है (२/१९)
"अतः उठो । वे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो मात्र बाह्य निमित्त बन जाओ।" (११/३३)
"जो व्यक्ति अहंभाव (कर्तृत्वभाव) से मुक्त है, इन लोगों को मार कर भी जिसकी बुद्धि प्रभावित नहीं होती, वह न तो मारता ही है और न ही कर्म-बन्धन में आता है।" (१८/१७) सार्वभौम सत्ता इन संकीर्ण मूल्यों से अतीत है।
साधक यदि आप्तकाम है, उसे भौतिक सुखों की अब कामना नहीं है, उसका चित्त शान्त है, उसके मन की अशुद्धि नष्ट हो चुकी है और वह निर्मल मन हो गया है, तो किसी भी सन्त पुरुष की शिक्षायें उसके हृदय को भेद कर ऐसे प्रभावित करती हैं जैसे शुद्ध, स्वच्छ और श्वेत वस्त्र को रंगीन जल । यही कारण है कि श्रवण, निदिध्यासन और ध्यान से पूर्व साधक से विवेक, वैराग्य, शम (मनोनिग्रह), दम (इन्द्रियनिग्रह), उपरति (विषयभोग से उदासीनता) का अभ्यास अपेक्षित है। सत्य और भगवत्साक्षात्कार के पथ पर चलने वाले साधकों से अनुशासन और मानस-शुद्धि पूर्वापेक्षित हैं।
परमात्मा के स्वभाव का जब कहीं वर्णन किया जाता है वहाँ भी वे लोग जिनकी बुद्धि पाप रहित और पवित्र नहीं होती, अविश्वास और आशंका के शिकार हो जाते हैं जैसा कि इन्द्र और विरोचन के साथ हुआ। इसलिए उपदिष्ट ज्ञानोदय तो केवल उसी व्यक्ति में होता है जिसने इसी जन्म में अथवा पूर्व-जन्म में तपश्चर्या से अघमर्षण कर लिया हो। श्रुति कहती है-"जिस महान् पुरुष की गुरु-भक्ति उतनी ही अधिक है जितनी भगवान् के प्रति, उसको यह सब ज्ञान निजात्मा में ही प्रकाशित हो जाता है।"
कुछ लोग अपनी रसना को शान्त करने के लिए गङ्गा नदी में मछली पकड़ते हैं और अपना बुरा कर्म उचित सिद्ध करने के लिए गीता का सहारा लेते हैं-"उसे शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकता" (२/२३)। कैसा अद्भुत दर्शन है! असुर भी शास्त्र को उद्धृत कर सकते हैं। ये लोग विरोचन के मतानुयायी हैं। वे अधम, मोहग्रस्त निकृष्ट मनुष्य हैं। वे गीता का ज्ञान नहीं समझ सकते; क्योंकि उनका विवेक आसुरी वृत्तियों को अपनाने के कारण भ्रमित हो गया है। भगवान् करे, उन्हें सूक्ष्म और पवित्र (निर्मल) बुद्धि प्राप्त हो! गीता के उपदेशों को सम्यक् प्रकार से समझने और उसी भाव में जीवन यापन करने के लिए उन्हें आभ्यन्तर, आध्यात्मिक शक्ति और विवेक प्राप्त हो!
कुछ अज्ञानी मनुष्यों का कथन है-"कृष्ण भगवान् नहीं हैं। वे अवतार नहीं हैं। वे वासनायुक्त गोपालक थे जिन्होंने काम-वासना में गोपियों के साथ क्रीड़ा की।" भगवान् कृष्ण की उस समय आयु क्या थी? क्या वे सात वर्ष के बालक नहीं थे? लेशमात्र भी काम-वासना उनमें हो सकती थी क्या? रासलीला और माधुर्यभाव (भक्त और भगवान् के मध्य प्रेम भाव), सर्वोच्च भक्ति की पराकाष्ठा, आत्म-निवेदन अथवा भगवान् के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण के रहस्य को कौन जान सकता है? नारद, शुकदेव, चैतन्य, मीरा, हफ़ीज़, रामानन्द, सखियाँ अथवा गोपियाँ ही इस रासलीला की महिमा और रहस्य को जान सके । तदर्थ सखियाँ ही प्रशिक्षित थीं। क्या बालावस्था में भगवान् कृष्ण ने चमत्कार नहीं दिखाये ? क्या उन्होंने यह नहीं दर्शाया कि वे स्वयं ही भगवान् विष्णु के अवतार थे? क्या शैशव काल में उन्होंने अपनी माताश्री को अपना अलौकिक रूप नहीं दिखाया ? क्या उन्होंने कालिय नाग के फण पर खड़े हो कर उसे वशीभूत नहीं किया? क्या उन्होंने स्वयं को अगणित कृष्ण रूपों में गुणित नहीं किया ? गोपियाँ कौन थीं? कृष्ण को सर्वत्र देखने वाली और स्वयं में कृष्ण के दर्शन करने वाली वे गोपियाँ भगवदुन्मत्त नहीं थीं? मुरली की धुन उन्हें दिव्य आनन्द अथवा पावन तादात्म्यता में पहुँचा देती थी। वे देहाध्यास से अतीत थीं।
भगवान् के लिए मिथ्या अपवाद करने और दोषदृष्टि रखने वालों की नियति क्या होगी? "मेरी अनुत्तम, अविनाशी, परा प्रकृति को न जानते हुए बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को व्यक्त भाव में आया समझते हैं" (७/२४)
“समस्त प्राणियों के महान् स्वामी अर्थात् मुझको मनुष्य रूप में अवतरित देख कर मेरी परात्पर प्रकृति से अनभिज्ञ मंदधी मनुष्य मेरा उपहास करते हैं। आशाशून्य, कर्मशून्य, ज्ञानशून्य वे लोग विक्षिप्त हो कर छाद्मिक, क्रूर (पशुतुल्य) और आसुर प्रकृति वाले हो जाते हैं" (९/११,१२) । “अज्ञानान्धकार से आवृत वे असत्य को सत्य मान कर पदार्थों को विपरीत भाव में देखते हैं। ऐसे आसुरी वृत्ति वाले न तो कर्म की परिभाषा जानते हैं, न त्याग की, न शुचिता की, न सदाचार की और न ही वे सत्य को जानते हैं, न ऋजुता को। किंकर्तव्यविमूढ़ ऐसे मनुष्यों को मैं आसुरी योनियों में डालता हूँ। मुझे न प्राप्त हो कर वे आवागमन के चक्र में फँस जाते हैं और निम्न योनियों को प्राप्त होते हैं" (१६/१९,२०)।
अनेक विचारशून्य व्यक्ति यह शंका करते हुए कहते हैं-"इतने अल्प समय में भगवान् ने समर भूमि में अर्जुन को गीता कैसे सुना दी? असम्भव, ऐसा नहीं हो सकता?" यह शंका अनुचित है। यह सब तो अर्जुन को श्रुति-प्रकाश हुआ । भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को सहजावबोध हेतु दिव्य चक्षु प्रदान किया। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् प्रभु कुछ भी करने में समर्थ हैं। उनकी कृपा हो तो मूक वाचाल बन जाये और पंगु पहाड़ पर चढ़ जाये ।
विप्रतिपन्न (विरुद्ध) श्लोकों का समाधान
एक विपक्षी लिखता है- "गीता के तीसरे अध्याय के ३३वें श्लोक में कहा गया है-'एक ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करता है। सभी प्राणी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। संयम क्या करेगा?' जब प्रकृति ही सर्वेसर्वा है, तो हमें मन तथा इन्द्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है? जब प्रकृति ही सर्वाधिक शक्तिशाली है, पराजित करने में समर्थ है, तो साधना उसे पराभूत कैसे कर सकती है?"
अगले श्लोक में भगवान् कृष्ण विशेष रूप से राग-द्वेष पर विजय पाने का उपदेश देते हैं। साधना से प्रकृति को संयत किया जा सकता है। गीताध्ययन करते समय केवल एक श्लोक के अर्थ में ही नहीं अटक जाना चाहिए । इसे तो न केवल उसी अध्याय के पूर्व और पश्चात् के श्लोकों से सम्बद्ध करना होगा, प्रत्युत् पूर्व के अध्याय भी ध्यान में रखने होंगे। विरुद्ध विषयों का सम्बन्ध बनाना होगा। तभी आपको समुचित उत्तर प्राप्त होगा।
भगवान् के आदेश की अवहेलना करके जो लोग कर्तव्य कर्म को त्याग कर शान्त बैठ जाते हैं, वे ऐसे त्याग से लाभान्वित नहीं हो सकते। तीसरे अध्याय ३०वें श्लोक में भगवान् का आदेश है-“सर्व कर्म मेरे समर्पण करके, आत्मस्थ (एकाग्रचित्त) हो कर, आशा और ममत्व को त्याग कर, मानसिक तनाव से मुक्त हो कर (हे अर्जुन), तुम युद्ध करो अर्थात् अपने कर्तव्य का पालन करो।" यह माया तो ज्ञानी पुरुषों के लिए भी अजेय है; फिर सांसारिक मनुष्य के लिए तो इसे जीतना और भी दुष्कर है। उनके लिए बिना ज्ञान प्राप्त किये कर्म-त्याग अपेक्षित नहीं है। वे माया के भँवर में फँस जायेंगे। उनके लिए इन्द्रियनिग्रह अथवा संयम का कोई प्रयोजन नहीं। सांसारिक मनुष्य राग-द्वेष से दूर नहीं रह सकते।
ज्ञानियों में अवशिष्ट सात्त्विक वासनायें भी, जो शरीर को स्थिर रखती हैं, प्रकृति के गुण-त्रय-सत्त्व, रजस् और तमस् के अनुरूप ही कार्य करते हैं। समाधि की यथार्थ अवस्था में न होने पर ये तीन गुण ज्ञानियों को भी प्रभावित करते हैं। उन्हें इस शरीर से अथवा अन्य भोग-विषयों में आसक्ति नहीं होती; अतः वे मानसिक रूप से प्रभावित नहीं होते। वे अपनी आत्मा में ही परितुष्ट और प्रशान्त होंगे। अनवाप्त विषयों को प्राप्त करने की उनमें आकाङ्क्षा नहीं होगी और न ही वे प्राप्त की हानि (लोप) पर शोक करेंगे।
आलोचक कहता है- "गीता के १८वें अध्याय के ६१वें श्लोक में भगवान् कृष्ण कहते हैं- 'हे अर्जुन! भगवान् सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और कुम्हार के चक्र पर आरूढ़ पात्र की भाँति अपनी माया से सबको भ्रमित करते हैं।' तो क्या मनुष्य पूर्ण रूप से परतन्त्र है? क्या वह तिनके की भाँति इधर से उधर ठुकरा दिया जाता है? क्या उसे कर्म की कोई स्वतन्त्रता नहीं है?"
भगवान् कृष्ण अर्जुन को अनुनीत करने का और उसकी शंकानिवारण का यथोचित प्रयास करते हैं जिससे कि वह अपने कर्म में संलग्न हो जाये। वे अर्जुन से काम लेना चाहते हैं; इसीलिए नितान्त असहाय अवस्था में वे उपदेश देते हैं। छठे अध्याय के ५वें श्लोक में भगवान् कृष्ण पुरुषार्थ का उपदेश देते हुए कहते हैं- “उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्-आत्मा से आत्मा का उद्धार करना है। आत्मा को अवसाद की स्थिति में नहीं ले जाना।"
प्रकृति के वश में होने के कारण स्वाभाविक गुणों का परित्याग नहीं हो सकता। कभी भी कर्तव्य-कर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान्, अन्तःकरण के स्वामी, व्यष्टि आत्मा के अनुशासक हैं। अविद्या के नाश होने पर्यन्त मनुष्य अपने धर्म (कर्तव्य-कर्म) से बँधा रहता है। अर्जुन क्षत्रिय है; अतः भगवान् चाहते हैं कि वह युद्ध में प्रवृत्त हो । अन्यत्र भगवान् कहते हैं : "श्रेयान् स्वधर्मः" -अपना कर्तव्य ही कल्याणप्रद है (१८/४७) ।
एक आलोचक का कथन १५वें अध्याय के ७वें श्लोक में भगवान् कृष्ण कहते हैं- 'इस जीव-जगत् में अमर आत्मा मेरा ही अंश है जो प्रकृति में अवगुंठित मन सहित छह इन्द्रियों को आकृष्ट करता है।' यह स्पष्ट है कि जीव ब्रह्म का अंश है, तो हम जीव को ब्रह्म का तद्रूप कैसे कह सकते हैं? अद्वैत सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण है।"
७वें अध्याय के १७वें श्लोक में भगवान् कहते हैं- "निश्चित रूप से ज्ञानी मेरे समान है।" यहाँ वे तद्रूपता की बात कर रहे हैं। अद्वैत सिद्धान्त समुचित ही है। सर्वोच्च साक्षात्कार अद्वैत स्थिति है। अधिकारी के अनुरूप ही भगवान् उपदेश करते हैं। अद्वैत दर्शन कतिपय सूक्ष्म बुद्धि वाले ही ग्रहण कर सकते हैं। अन्य साधकों की रुचि का ध्यान रखते हुए अन्य दर्शनों की व्याख्या वे अन्य स्थानों पर करते हैं। पूर्णत्व के दृष्टिकोण से न तो जीव की सत्ता है और न साक्षात्कार की। वस्तुतः एक ब्रह्म ही का केवल अस्तित्व है। द्वैत (dualism), विशिष्टाद्वैत (qualified monism), शुद्ध अद्वैत (pure monism) साक्षात्कार की सीढ़ी के पृथक् पृथक् सोपान हैं। सत्य यही है कि साररूप में जीव और ब्रह्म एक हैं। द्वैतवादी और विशिष्टाद्वैतवादी अन्ततः अद्वैत के लक्ष्य अथवा एकत्व के साक्षात्कार को ही प्राप्त करते हैं। भ्रम में न पड़ें। विचारों को स्पष्ट करें और समुचित विचारधारा के प्रकाश में ज्ञान प्राप्त करें।
उपसंहार
पाश्चात्य देशवासियों द्वारा भारत देश को गीता के कारण महान् गौरव प्राप्त हुआ है। एक बार महात्मा गान्धी लन्दन के एक बड़े पुस्तकालय में गये और ग्रन्थाध्यक्ष से पूछा- "कौन-से आध्यात्मिक ग्रन्थ का सर्वाधिक निष्कासन होता है?" अध्यक्ष ने कहा- "गीता।" संसार भर में गीता को ख्याति प्राप्त है। सभी साधकों को इस विश्वविख्यात ग्रन्थ के सम्पूर्ण अठारह अध्याय कण्ठस्थ कर लेने चाहिए। नित्य स्वाध्याय और प्रतिदिन दो श्लोक कण्ठस्थ कर लेने से लगभग दो वर्षों में यह कार्य सम्पन्न हो सकता है।
भारत ही नहीं प्रत्युत् विश्व की समस्त पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों में गीता का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। समस्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गीता को पाठ्यपुस्तक (Textbook) का स्थान मिलना चाहिए। उनके अध्ययन क्रम (curriculum) में इसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। शिक्षा की प्रत्येक प्रणाली में इसे महत्त्वपूर्ण स्थान उपलब्ध होना चाहिए। लौकिक ज्ञान के साथ-साथ जिसमें नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, वही शिक्षा-पद्धति सुदृढ़, व्यावहारिक, विषयबोधगम्य और पूर्ण मानी जाती है।
आपमें से प्रत्येक को इस उत्कृष्ट, मार्मिक ग्रन्थ का अध्ययन सावधानी से करना चाहिए। यह परम शान्ति, अमृतत्व और शाश्वत आनन्द की वृष्टि करने वाला ग्रन्थ है।
विश्वास का दीप जलाओ । शान्ति की इस अद्भुत पताका को वायु में ऊँचा लहराने दो। अनासक्ति का महान् कवच धारण करो। विवेक का अलौकिक शस्त्र उठाओ। 'सोऽहम्', 'शिवोऽहम्', किंवा 'राधेश्याम', 'सीताराम' का अमर गीता गाओ । ॐ ॐ के प्रणव बैण्ड के साथ वीरतापूर्वक आगे बढ़ो । साहस का अनोखा शंख बजाओ । शंका, अविद्या, आसक्ति, अहं आदि शत्रुओं का विनाश करके आत्मा के अनन्त साम्राज्य में प्रवेश करो। दिव्य अमृतरस का आस्वादन करो। अमृतत्व का सुधारस पान करो।
भगवान् गणेश, भगवान् सुब्रह्मण्यम्, भगवान् राम, देवी सीता, श्री सरस्वती, श्री भगवान् व्यास, श्री आदि शंकराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, त्रोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, श्री ज्ञानदेव, श्री स्वामी विश्वानन्द, श्री स्वामी विष्णुदेवानन्द, ब्रह्मविद्या के समस्त गुरुओं, सन्तों, आचायर्यों, भगवद्गीता के समस्त टीकाकारों को मेरा मौन प्रणाम, जिनकी अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद के कारण ही मैं भगवद्गीता पर टीका लिखने में समर्थ हुआ। आप सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो!
भगवद्रीता की जय हो! भगवान् कृष्ण की जय हो जिन्होंने मनुष्यों के कल्याणार्थ अथवा उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए गीता का ज्ञान विश्व के समक्ष रखा ! आप सब पर उनकी कृपा-वृष्टि हो ! गीता तुम्हारा लक्ष्य, आदर्श और केन्द्र हो ! गीता का नित्य अध्ययन करने वाला पुरुष धन्य है ! दुगना धन्य वह पुरुष है जो गीता के भाव में जीता है ! तिगुना धन्य वह है जिसने गीता-ज्ञान का साक्षात्कार कर आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया है !
ॐ तत् सत्!
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !
-स्वामी शिवानन्द
विषय-सूची
अध्याय-1
अध्याय-2
अध्याय-3
अध्याय-4
अध्याय-5
अध्याय-6
अध्याय-7
अध्याय-8
अध्याय-9
अध्याय-10
अध्याय-11
अध्याय-12
अध्याय-13
अध्याय-14
अध्याय-15
अध्याय-16
अध्याय-17
अध्याय-18
|
श्लोक में सज्जित शब्दों के अर्थ उसी क्रम में दिये गये हैं और अनुवाद में सहज गद्य-पद्यति अपनायी गयी है।
|
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ प्रथमोऽध्यायः
अर्जुनविषादयोगः
धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ।। १ ।।
शब्दार्थ : धर्मक्षेत्रे -धर्मभूमि में, कुरुक्षेत्रे-कुरुक्षेत्र में, समवेताः- एकत्रित, युयुत्सवः-युद्ध की इच्छा वाले, मामकाः- मेरे (पक्ष के), पाण्डवाः- पाण्डु पुत्रों ने, च-और, एव-ही, किम् -क्या, अकुर्वत-किया, सञ्जय-हे सञ्जय ।
धृतराष्ट्र ने कहा
अनुवाद : हे सञ्जय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया ?
व्याख्या : धर्मक्षेत्र-वह क्षेत्र अथवा स्थान, जहाँ धर्म की रक्षा होती है ।
कुरुक्षेत्र-कौरवों के राज्य में होने के कारण यह स्थल कुरुक्षेत्र कहलाया।
सञ्जय वह है, जिसने इच्छा-अनिच्छा आदि द्वन्द्वों को जीत लिया है और निष्पक्ष है।
सञ्जय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ।।२ ।।
शब्दार्थ : दृष्ट्वा-देख कर, तु-निश्चित रूप से, पाण्डवानीकम् -पाण्डवों की सेना को, व्यूढम् - व्यूह रचना, दुर्योधनः दुर्योधन, तदा-तब, आचार्यम्-आचार्य, उपसङ्गम्य-समीप जा कर, राजा-राजा, वचनम्-वचन (शब्द), अब्रवीत् -बोला।
सञ्जय ने कहा
अनुवाद : पाण्डवों की सेना को व्यूह (सेना का विन्यास विशेष) में खड़ा देख कर राजा दुर्योधन आचार्य के समीप जा कर यह वचन बोला।
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।
न्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ।।३ ।।
शब्दार्थ : पश्य-देखो, एताम् - इसे, पाण्डुपुत्राणाम् -पाण्डुपुत्रों की, आचार्य-हे आचार्य, महतीम् -महान्, चमूम् -सेना, व्यूढाम्-व्यूढाकार में व्यवस्थित, द्रुपदपुत्रेण -द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव शिष्येण - आपके शिष्य के द्वारा, धीमता-बुद्धिमान् ।
अनुवाद : हे आचार्य, आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपद के पुत्र (धृष्टद्युम्न) द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की गयी पाण्डु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखो।
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ।।४।।
शब्दार्थ : अत्र-यहाँ, शूराः-वीर, महेष्वासाः - महान् धनुर्धर, भीमार्जुनसमाः - भीम और अर्जुन के समान, युधि-युद्ध में, युयुधानः - युयुधान, विराटः-विराट, च-और, द्रुपदः द्रुपद, च-और, महारथः - महारथी।
अनुवाद : "यहाँ (इस सेना में) भीम और अर्जुन के समान महान् योद्धा और धनुर्धर हैं। युयुधान (सात्यकि), विराट् और द्रुपद जैसे महारथी हैं।
व्याख्या : महारथः - परिभाषा की दृष्टि से इसका अर्थ है वह योद्धा जो युद्धविज्ञान में कुशल हो और अकेला ही दश सहस्र धनुर्धरों से लड़ने की क्षमता रखता हो ।
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ।।५ ।।
शब्दार्थ : धृष्टकेतुः- धृष्टकेतु, चेकितानः- चेकितान, काशिराजः-काशी नरेश, च-और, वीर्यवान् वीर, पुरुजित् -पुरुजित, कुन्तिभोजः-कुन्तिभोज, च-और, शैब्यः-शिवि का पुत्र, च-और, नरपुङ्गवः- मनुष्यों में श्रेष्ठ ।
अनुवाद : "धृष्टकेतु, चेकितान और बलशाली काशी नरेश, पुरुजित् और कुन्तिभोज तथा नरश्रेष्ठ शैब्य ।
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ।।६ ।।
शब्दार्थ : युधामन्युः युधामन्यु, च-और, विक्रान्तः-शक्तिशाली, उत्तमौजाः उत्तमौजस्, च-और, वीर्यवान् वीर, सौभद्रः सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेयाः द्रौपदी के पुत्र, च-और, सर्वे-सभी, एव-ही, महारथाः- महान् योद्धा ।
अनुवाद : "शक्तिशाली युधामन्यु और वीर उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र (अभिमन्यु) तथा द्रौपदी के पाँचों पुत्र-यह सब महारथी हैं।
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ।।७ ।।
शब्दार्थ : अस्माकम् -हमारे, तु-भी, विशिष्टाः-सर्वश्रेष्ठ, ये-जो, तान्-उनका, निबोध-जानलो, द्विजोत्तम-ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायकाः-नायक, मम-मेरी, सैन्यस्य-सेना के, संज्ञार्थम् -सूचना के लिए, तान् उनको, ब्रवीमि बताता हूँ, ते-आपको ।
अनुवाद : "हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! हमारी सेना में भी जो उत्कृष्ट नायक हैं उन्हें आप जान लीजिए, आपकी सूचना के लिए मैं उनके नाम बताता हूँ।
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः ।
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ।।८ ।।
शब्दार्थ : भवान् - आप, भीष्मः-भीष्म, च-और, कर्ण:-कर्ण, च-और, कृपः -कृपाचार्य, च-और, समितिञ्जयः - युद्ध में विजयी, अश्वत्थामा-अश्वत्थामा (द्रोणाचार्य का पुत्र), विकर्णः - विकर्ण, च-और, सौमदत्तिः सोमदत्त का पुत्र, तथा- इस प्रकार, एव-ही, च-और।
अनुवाद : "आप और भीष्म, कर्ण और संग्राम-विजेता कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ।।९ ।।
शब्दार्थ : अन्ये-अन्य (दूसरे), च और, बहवः अनेक, शूराः शूरवीर, मदर्थे -मेरे लिए, त्यक्तजीविताः- जीवनोत्सर्ग करने को उद्यत, नानाशस्त्रप्रहरणाः -नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित, सर्वे-सब, युद्धविशारदाः - युद्ध कला में निपुण।
अनुवाद : "और भी अनेक ऐसे योद्धा हैं जो युद्धकला में निपुण तथा नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। वे सब मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ।।१० ।।
शब्दार्थ : अपर्याप्तम् - अपर्याप्त, तत्-वह, अस्माकम् -हमारी, बलम् -सेना, भीष्माभिरक्षितम् - भीष्मपितामह द्वारा रक्षित, पर्याप्तम् - पर्याप्त, तु-जब कि, इदम् यह, एतेषाम् - उनकी, बलम् -सेना, भीमाभिरक्षितम् - भीम द्वारा रक्षित ।
अनुवाद : "भीष्मपितामह के संरक्षण में हमारी सेना अपर्याप्त (अप्रचुर) है जब कि भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त (प्रचुर) है।
व्याख्या : टीकाकारों ने इस श्लोक की व्याख्या भिन्न-भिन्न रूप से की है। श्रीधर स्वामी के अनुसार 'अपर्याप्तम्' का अर्थ है- अप्रचुर अथवा अल्प जब कि आनन्दगिरि इस शब्द को 'असीमित' भाव में लेते हैं।
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ।।११ ।।
शब्दार्थ : अयनेषु -चक्रव्यूहों में (सेना के), च-और, सर्वेषु सभी, यथाभागम् - अपने-अपने भाग (स्थान और दल) के अनुरूप, अवस्थिताः -खड़े रह कर, भीष्मम् -भीष्म की, एव-केवल, अभिरक्षन्तु-रक्षा करें, भवन्तः - आप सब, सर्वे-सभी, एव-ही, हि-निश्चित रूप से।
अनुवाद : "इसलिए आप सब अपने-अपने स्थान पर स्थित रह कर सेना के सभी व्यूहों में सब ओर से केवल भीष्मपितामह की ही रक्षा करें।"
तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।
सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखंदध्मौ प्रतापवान् ।।१२ ।।
शब्दार्थ : तस्य-उसका (दुर्योधन का), संजनयन् -बढ़ाते हुए, हर्षम् -हर्ष, कुरुवृद्धः-कौरवों में वयोवृद्ध, पितामहः-पितामह, सिंहनादम् - सिंह की गर्जना, विनद्य -गरज कर, उच्चैः- उच्च स्वर से, शंखम् -शंख, दध्मौ-बजाया, प्रतापवान् - प्रतापी ।
अनुवाद : कुरुवृद्ध महातेजस्वी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह के समान गरज कर उच्च स्वर से अपना शंख बजाया।
ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ।।१३ ।।
शब्दार्थ : ततः-तत्पश्चात्, शंखाः-शंख, च-और, भेर्यः भेरी (दुंदुभि), च-और, पणवानकगोमुखाः-ढोल, मृदङ्ग और सींग (शृङ्ग), सहसा एव-अकस्मात् ही, अभ्यहन्यन्त-उद्घोष हुआ, सः- वह, शब्दः- ध्वनि, तुमुलः- भयंकर, अभवत् था ।
अनुवाद : तत्पश्चात् (भीष्म का अनुसरण करते हुए), शंख, दुंदुभि, ढोल, मृदङ्ग और शृङ्ग बाजों का सहसा ही उद्घोष हुआ। वह नाद अत्यन्त भयंकर था।
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ।।१४।।
शब्दार्थ : ततः-तत्पश्चात्, श्वेतैः- श्वेत, हयैः-घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति-विशाल, स्यन्दने-रथ में, स्थितौ-बैठे हुए, माधवः- माधव (कृष्ण), पाण्डवः-पाण्डव (पाण्डुपुत्र), च-और, एव-ही, दिव्यौ-दिव्य, शंखौ शंख, प्रदध्मतुः बजाये ।
अनुवाद : तदुपरान्त, श्वेत घोड़ों से युक्त अतिशोभन (विशाल) रथ में विराजित माधव (कृष्ण) और पाण्डुपुत्र (अर्जुन) ने अपने-अपने दिव्य शंखों से नाद किया।
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
पौण्डूं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ।।१५।।
शब्दार्थ : पाञ्चजन्यम् -पाञ्चजन्य नामक शंख, हृषीकेशः इन्द्रियों के स्वामी (कृष्ण), देवदत्तम् - देवदत्त (शंख का नाम), धनञ्जयः-कुबेर को जीतने वाले (अर्जुन), पौण्ड्रम् -पौण्ड्र नामक शंख, दध्मौ-बजाया, महाशंखम् -महान् शंख, भीमकर्मा-भयंकर कार्य करने वाले, वृकोदरः- भीम (भेड़िये के समान उदर वाला)।
अनुवाद : भगवान् कृष्ण ने पाञ्चजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले, अति भोजी भीम ने पौण्ड्र शंख बजाया ।
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ।।१६ ।।
शब्दार्थ : अनन्तविजयम् - अनन्तविजय नामक शंख, राजा-राजा, कुन्तीपुत्रः कुन्तीपुत्र, युधिष्ठिरः- युधिष्ठिर, नकुलः- नकुल, सहदेवः सहदेव, च-और, सुघोषमणिपुष्पकौ-सुघोष और मणिपुष्पक (शंख)।
अनुवाद : कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाये।
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ।।१७ ।।
शब्दार्थ : काश्यः-काश्य (काशी नरेश), च-और, परमेष्वासः-उत्कृष्ट धनुर्धर, शिखण्डी-शिखण्डी, च-और, महारथः महान् योद्धा, धृष्टद्युम्नः- धृष्टद्युम्न, विराटः-विराट, च-और, सात्यकिः-सात्यकि (युयुधान, श्रीकृष्ण का सारथी), च-और, अपराजितः - अजेय ।
अनुवाद : महान् धनुर्धर काश्य (काशी नरेश), महान् योद्धा शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकि ने,
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक्पृथक् ।।१८ ।।
शब्दार्थ : द्रुपदः द्रुपद, द्रौपदेयाः - द्रौपदी के पुत्र, च और, सर्वशः-सब, पृथिवीपते-हे पृथिवीपति, सौभद्रः-सुभद्रा का पुत्र (अभिमन्यु), च-और, महाबाहुः-विशाल भुजाओं वाला, शंखान्-शंख, दध्मुः बजाये, पृथक् पृथक् अलग-अलग।
अनुवाद : हे वसुन्धरा के स्वामी! द्रुपद और द्रौपदी के सभी पुत्रों ने तथा महाबाहु अभिमन्यु ने पृथक् पृथक् शंख बजाये ।
व्याख्या : इस शंखनाद ने युद्ध के आरम्भ होने की घोषणा की।
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ।।१९ ।।
शब्दार्थ : सः-उस, घोषः -नाद ने, धार्तराष्ट्राणाम् - धृतराष्ट्र के पुत्रों के, हृदयानि-हृदय, व्यदारयत्-विदीर्ण कर दिये, नभः- आकाश, च-और, पृथिवीम् -पृथिवी को, च-और, एव-भी, तुमुलः- भयानक, व्यनुनादयन् - प्रतिध्वनित करते हुए।
अनुवाद : पृथिवी लोक और द्युलोक को प्रतिध्वनित करते हुए उस भयानक शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पक्ष के सैनिकों के हृदय विदीर्ण कर दिये।
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।।२० ।।
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।
शब्दार्थ : अथ-अब, व्यवस्थितान् - व्यूह में खड़े हुए, दृष्ट्वा देख कर, धार्तराष्ट्रान् - धृतराष्ट्र के पक्ष को, कपिध्वजः- हनुमान् जी के चित्र से चित्रित पताका, प्रवृत्ते-प्रारम्भ करने को उद्यत, शस्त्रसंपाते-शस्त्र चलाने के लिए, धनुः- धनुष, उद्यम्य-उठा कर, पाण्डवः -पाण्डुपुत्र, हृषीकेशम् -हृषीकेश (कृष्ण) को, तदा-तब, वाक्यम्-वचन, इदम्-यह, आह-कहा, महीपते- हे राजन्।
अनुवाद : कपिध्वज से सुशोभित रथ पर आसीन अर्जुन धृतराष्ट्र के पक्ष की सेना को व्यूह में खड़ा देख कर शस्त्रास्त्र चलाने को उद्यत हुआ और अपने धनुष को उठा कर भगवान् कृष्ण से बोला- हे महीपते!
अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।।२१ ।।
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् ।
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ।।२२ ।।
शब्दार्थ : सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों, मध्ये-बीच में, रथम् रथ को, स्थापय-खड़ा करें, मे-मेरे, अच्युत-अच्युत (सदा एकरस, कृष्ण), यावत् जब तक, एतान् - इन्हें, निरीक्षे-देख लूँ, 3784 - 4 योद्धकामान् युद्ध की इच्छा वाले, अवस्थितान् -स्थित, कै:-किन के साथ, मया-मेरे द्वारा, सह-साथ, योद्धव्यम् - युद्ध करना है, अस्मिन् - इसमें, रणसमुद्यमे-रण के प्रयास में अथवा युद्ध प्रारम्भ होने की तैयारी में।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे कृष्ण ! कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दें जिससे मैं युद्ध प्रारम्भ होने की इस वेला में युद्ध की आकाङ्क्षा वाले लोगों को देख सकूँ और जान सकूँ कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है।
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ।।२३ ।।
शब्दार्थ : योत्स्यमानान् - युद्ध की इच्छा वालों को, अवेक्षे-देख लूँ, अहम् -मैं, ये जो, एते-वे, अत्र-यहाँ (कुरुक्षेत्र में), समागताः- एकत्रित, धार्तराष्ट्रस्य-धृतराष्ट्र के पुत्र, दुर्बुद्धेः- दुष्ट बुद्धि वाले, 46 - 9% प्रियचिकीर्षवः- हित चाहने वाले ।
अनुवाद : दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले युद्ध की कामना से यहाँ आये हुए लोगों को देख लूँ।
सञ्जय उवाच
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ।।२४ ।।
शब्दार्थ : एवम् - इस प्रकार, उक्तः-कहे गये, हृषीकेशः-कृष्ण, गुडाकेशेन-गुडाकेश के द्वारा (अर्जुन, जिसने निद्रा को वश में कर लिया), भारत-है भारत (भरतवंशी धृतराष्ट्र), सेनयोः - सेनाओं के, उभयोः - दोनों, मध्ये-बीच में, स्थापयित्वा खड़ा करके, रथोत्तमम् -सर्वोत्कृष्ट रथ को ।
सञ्जय ने कहा
अनुवाद : हे भारत! अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान् कृष्ण ने उस सर्वोत्कृष्ट रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर के-
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान्कुरूनिति ।। २५ ।।
शब्दार्थ : भीष्मद्रोणप्रमुखतः - भीष्म और द्रोण के समक्ष, सर्वेषाम् -सब के, च-और, महीक्षिताम् - राजाओं के, उवाच-कहा, पार्थ-हे अर्जुन, पश्य-देखो, एतान् -इन्हें, समवेतान् - एकत्रित हुए, कुरून् कुरुवंशियों को, इति-इस प्रकार ।
अनुवाद : भीष्म, द्रोण और सभी राजाओं के समक्ष कहा- हे अर्जुन (पृथापुत्र), यहाँ एकत्रित कुरुवंशियों को देखो ।
तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ।
आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ।। २६ ।।
शब्दार्थ : तत्र-वहाँ, अपश्यत्-देखा, स्थितान् -स्थित, पार्थः-अर्जुन ने, पितृन् -पितरों को, अथ-भी, पितामहान् -पितामहों को, आचार्यान् - गुरुजनों को, मातुलान् मामाओं को, भ्रातृन् - भाइयों को, पुत्रान् -पुत्रों को, पौत्रान् -पौत्रों को, सखीन् -मित्रों को, तथा और।
अनुवाद : अर्जुन ने वहाँ (सेनाओं के मध्य) पिता, पितामह, गुरुजन, मामा, भ्राता, पुत्र, पौत्र तथा मित्रगणों को देखा।
श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ।। २७ ।।
कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।
शब्दार्थ : श्वशुरान् -श्वसुरों को, सुहृदः-शुभचिन्तक (मित्र), च-और, एव-भी, सेनयोः सेनाओं में, उभयोः दोनों (में), अपि-भी, तान् उन्हें, समीक्ष्य-देख कर, सः वह, कौन्तेयः कुन्ती पुत्र अर्जुन, सर्वान् सभी, बन्धून् सम्बन्धी, अवस्थितान् - व्यूह में खड़े हुए, कृपया-दया भाव से, परया-गहन, आविष्टः- अभिभूत, विषीदन्-व्याकुल हो कर, इदम् यह, अब्रवीत् कहा।
अनुवाद : (अर्जुन ने) श्वसुरों और शुभचिन्तकों को भी दोनों सेनाओं के मध्य देखा। उन सभी बन्धु-बान्धवों (सम्बन्धियों) को (समक्ष) खड़ा देख कर अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा और वह व्याकुल हो कर बोला-
अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ।।२८ ।।
शब्दार्थ : दृष्ट्वा -देख कर, इमम्-इन्हें, स्वजनम् -स्वजनों को, कृष्ण-हे कृष्ण (श्याम वर्ण, जो आकृष्ट करता है), युयुत्सुम-लड़ने को आतुर, समुपस्थितम् - खड़े हुए।
अनुवाद : युद्ध की इच्छा से आये हुए इन सम्बन्धियों को देख कर हे कृष्ण,
अर्जुन ने कहा
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।।२९ ।।
शब्दार्थ : सीदन्ति-शिथिल हो रहे हैं, मम-मेरे, गात्राणि-अङ्ग, मुखम् -मुख, च-और, परिशुष्यति-सूख रहा है, वेपथुः कम्पन, च-और, शरीरे शरीर में, मे मेरे, रोमहर्ष:-रोमांच, च-और, जायते-हो रहा है।
अनुवाद : मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर काँप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
गाण्डीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।। ३० ।।
शब्दार्थ : गाण्डीवम् - गाण्डीव, संसते-गिरा जा रहा है, हस्तात् - हाथ से, त्वक् त्वचा, च-और, एव-भी, परिदह्यते-जल रही है, न नहीं, च-और, शक्नोमि-समर्थ हूँ, अवस्थातुम् - खड़े होने में, भ्रमति इव-भ्रमित सा हो रहा है, च-और, मे मेरा, मनः मन ।
अनुवाद : गाण्डीव (धनुष) हाथ से छूटा जा रहा है, सारी त्वचा भी जल रही है, मन भ्रमित सा हो रहा है और अब मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।। ३१ ।।
शब्दार्थ : निमित्तानि-लक्षण (शुभाशुभ), च-और, पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि-अशुभ, केशव-हे केशव, न-नहीं, च-और, श्रेयः-कल्याण, अनुपश्यामि -देखता हूँ, हत्वा-मार कर, स्वजनम्-अपने लोगों को, आहवे- युद्ध में।
अनुवाद : हे केशव ! इस युद्ध में अपने ही सम्बन्धियों को मार कर मुझे किसी का कल्याण होता तो दृष्टिगत नहीं हो रहा, प्रत्युत् मुझे अपशकुन (अशुभ लक्षण) दिखायी दे रहे हैं।
व्याख्या : केशव का अर्थ है-सुन्दर, संवर्धित बालों वाला।
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।। ३२ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, काङ्क्ष-कामना करता हूँ, विजयम् - विजय, कृष्ण-हे कृष्ण, न-नहीं, च-और, राज्यं -राज्य, सुखानि -सुख, च-और, किम् -क्या, नः- हमें, राज्येन-राज्य से, गोविन्द- हे गोविन्द, किम् -क्या, भोगैः- भोगों से, जीवितेन-जीवन से, वा-अथवा ।
अनुवाद : हे कृष्ण ! न तो मुझे विजय की अभिलाषा है, न राज्य की और न ही सुखों की। हे गोविन्द ! हमें राज्य से अथवा सुख-भोग से क्या लाभ ? पुनश्च इस जीवन से भी क्या प्रयोजन ?
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।। ३३ ।।
शब्दार्थ : येषाम् -जिनके, अर्थे-लिए, काङ्क्षितं - इच्छित, नः- हमारे द्वारा, राज्यम् -राज्य, भोगाः-सुख-भोग, सुखानि-समस्त सुख, च-और, ते-वे, इमे-ये, अवस्थिताः-खड़े हैं, युद्धे -रणक्षेत्र में, प्राणान् - प्राणों को, त्यक्त्वा-त्याग कर, धनानि-सम्पत्ति, च-और।
अनुवाद : जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की आकाङ्क्षा करते हैं, वे सब अपने जीवन और सम्पत्ति का मोह त्याग कर युद्ध में आ खड़े हैं।
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ।।३४ ।।
शब्दार्थ : आचार्याः -गुरुजन, पितरः-पितृगण, पुत्राः-पुत्र, तथा-तथा, एव-ही, च-और, पितामहाः-पितामह, मातुला:-मामा, श्वशुराः -श्वशुर, पौत्राः-पौत्र, श्यालाः-साले, सम्बन्धिनः-सम्बन्धी, तथा-और, अन्य।
अनुवाद : गुरुजन, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, श्याले (साले) और अन्य सम्बन्धी-
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ।। ३५ ।।
शब्दार्थ : एतान् -इन्हें, न-नहीं, हन्तुम्-मारने के लिए, इच्छामि -इच्छा करता हूँ, घ्नतः अपि-मारे जाने पर भी, मधुसूदन-हे मधुसूदन (मधु राक्षस का वध करने वाले), अपि-भी, त्रैलोक्यराज्यस्य-तीनों लोकों के राज्य, हेतोः के लिए, किम् -कैसे, नु-फिर, महीकृते-धरा (के राज्य) के लिए।
अनुवाद : हे मधुसूदन! मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं रखता, भले ही वे मुझे मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं ऐसी इच्छा नहीं कर सकता फिर इस धरती के साम्राज्य की तो बात ही क्या?
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ।।३६ ।।
शब्दार्थ : निहत्य-मार कर, धार्तराष्ट्रान् - धृतराष्ट्र के पुत्रों को, नः हमें, का-क्या, प्रीतिः -सुख, स्यात् -होगा, जनार्दन- हे जनार्दन, पापम् -पाप, एव--केवल, आश्रयेत् - लगेगा, अस्मान् -हमें, हत्वा-मार कर, एतान् -इनको, आततायिनः - दुष्टों को ।
अनुवाद : धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हे जनार्दन, हमें कौन से सुख की प्राप्ति होगी? इन दुष्टों की हत्या से तो हम केवल पाप के ही भागी बनेंगे।
व्याख्या : जनार्दन-ऐश्वर्य-समृद्धि और मोक्ष के लिए जो सबका आराध्य है-कृष्ण ।
आततायी-जो दूसरों के घर को आग लगा देता है, दूसरों को विष देता है, खड्ग ले कर मारने को उद्यत रहता है, धन लूटता है, भूमि का अपहरण करता है, और जो दूसरे की पत्नी पर अधिकार जमाता है। दुर्योधन ने ये सभी दुष्कर्म किये थे।
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् ।
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।। ३७ ।।
शब्दार्थ : तस्मात् - इसलिए, न-नहीं, अर्हाः- युक्त, वयम् -हम सब, हन्तुम् -मारने के लिए, धार्तराष्ट्रान् - धृतराष्ट्र के पुत्रों को, स्वबान्धवान्-अपने सम्बन्धियों को, स्वजनम् -सम्बन्धी (मित्रगण), हि-निश्चय से, कथम् -किस प्रकार, हत्वा -मार कर, सुखिनः-सुखी, स्याम-होंगे, माधव- हे माधव ।
अनुवाद : अतः अपने ही भाई-बन्धु, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए युक्त नहीं है; क्योंकि हे माधव, अपने ही लोगों (प्रियजनों) को मार कर हम सुखी कैसे हो सकते हैं?
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ।।३८ ।।
शब्दार्थ : यद्यपि -यद्यपि (यदि+अपि), एते-ये, न-नहीं, पश्यन्ति- देखते हैं, लोभोपहतचेतसः- लोभ के वशीभूत चित्त वाले, कुलक्षयकृतम् -कुल के नष्ट होने पर, दोषम् -पाप को, मित्रद्रोहे-मित्र के साथ द्रोह करने में, च-और, पातकम् -पाप को।
अनुवाद : यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग न तो कुल के विनाश में कोई दोष देख रहे हैं और न ही मित्रद्रोह में कोई पाप मान रहे हैं।
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ।।३९ ।।
शब्दार्थ : कथम् -क्यों, न-नहीं , ज्ञेयम्-समझना चाहिए, अस्माभिः- हमें (हमारे द्वारा), पापात् -पाप से, अस्मात् - इस, निवर्तितुम् - निराकरण हेतु, कुलक्षयकृतम् -कुल के विनाश से उद्भूत, दोषम् -बुराई, प्रपश्यद्भिः-स्पष्ट देखते हुए, जनार्दन-हे जनार्दन ।
अनुवाद : किन्तु हे जनार्दन, कुल के विनाश से उत्पन्न होने वाली बुराइयों को हम तो स्पष्ट देख रहे हैं तो इस पाप को दूर करने का ज्ञान हमें तो होना चाहिए।
व्याख्या : नियम का अज्ञान कोई व्यपदेश (बहाना) नहीं है; किन्तु विलासवत् पापी चरित्र महान् अपराध है, हमें ऐसा करना उचित नहीं है जो कि उनसे अधिक बुद्धिमान् हैं।
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ।।४० ।।
शब्दार्थ : कुलक्षये-कुल के विनाश में, प्रणश्यन्ति-नष्ट हो जाते हैं, कुलधर्माः-पारिवारिक धार्मिक परम्परायें, सनातनाः-शाश्वत, धर्म-धर्म, नष्टे -नष्ट होने पर, कुलं कृत्स्नम् -समस्त कुल, अधर्मः-अधर्म, अभिभवति-हावी हो जाता है, उत-निश्चित रूप से ।
अनुवाद : कुल का विनाश होने पर उस कुल के शाश्वत धार्मिक विधि-विधान नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर समस्त कुल में अधर्म का साम्राज्य हो जाता है।
व्याख्या : शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप परिवार में किया जाने वाला यज्ञादि कर्तव्य कर्म ही धर्म है।
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्र्णेय जायते वर्णसंकरः ।।४१ ।।
शब्दार्थ : अधर्माभिभवात् - (अधर्म+अभिभवात्) अधर्म का प्रसार होने से, कृष्ण-हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति-दूषित हो जायेंगी, कुलस्त्रियः-कुल की स्त्रियाँ, स्त्रीषु-स्त्रियों में, दुष्टासु-दुष्ट होने पर, वार्णेय - हे वाष्र्णेय, जायते-उत्पन्न होता है, वर्णसंकरः जाति-मिश्रण।
अनुवाद : हे कृष्ण! अधर्म के प्रसार से कुलीन स्त्रियाँ भ्रष्ट हो जायेंगी और स्त्रियों के भ्रष्ट होने पर हे वाष्र्णेय (वृष्णी वंशी), पृथक् जातियों का मिश्रण हो जायेगा।
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।।४२ ।।
शब्दार्थ : संकरः- जाति-मिश्रण, नरकाय-नरक के लिए, एव-ही, कुलघ्नानाम् -कुलघातियों के, कुलस्य-परिवार के, च-और, पतन्ति-गिर जाते हैं, पितरः-पूर्वज, हि-निश्चय से, एषाम् -इनके, लुप्तपिण्डोदकक्रियाः- (श्राद्ध में पितरों को दिया जाने वाला) चावल के पिण्ड का दान और जल के अर्पण की क्रिया का लुप्त होना।
अनुवाद : वर्णसंकर कुल तथा कुल को नष्ट करने वालों के लिए नरक का द्वार है; क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्मायें पिण्डदान और जल-तर्पण की क्रिया लुप्त होने पर अन्न-जल से वंचित हो कर गिर पड़ती हैं।
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।।४३ ।।
शब्दार्थ : दोषैः -दोषों (बुराइयों) से, एतैः-इन (के कारण), कुलघ्नानाम् -कुल को नष्ट करने वालों के, वर्णसंकरकारकैः- जाति-मिश्रण के हेतुक, उत्साद्यन्ते-नष्ट हो जाते हैं, जातिधर्माः- जातिधर्म, कुलधर्माः-कुल में होने वाले धर्मिक अनुष्ठान, च-और, शाश्वताः- सनातन ।
अनुवाद : कुलघातियों के द्वारा किये गये, वर्णसंकर के हेतुक, दोषों से, सनातन जातिधर्म और कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं।
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ।।४४ ।।
शब्दार्थ : उत्सन्नकुलधर्माणाम् -जिनके कुलधर्म (पारम्परिक अनुष्ठान) नष्ट हो चुके हों, मनुष्याणाम् - मनुष्यों के, जनार्दन-हे जनार्दन, नरके-नरक में, अनियतम् -चिरकाल तक, वासः - निवास, भवति - होता है, इति-इस प्रकार, अनुशुश्रुम-हमने सुना है।
अनुवाद : हे जनार्दन ! हमने सुना है कि जिनके परिवारों में कुलधर्म विनष्ट हो जाते हैं, उनका चिरकाल पर्यन्त नरक में वास होता है।
अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ।।४५ ।।
शब्दार्थ : अहो बत-हा, आश्चर्य, महत्-महान्, पापम् -पाप, कर्तुम् -करने के लिए, व्यवसिताः-तैयार, वयम् -हम, यत् - कि, राज्यसुखलोभेन राज्य के सुख के लोभवश, हन्तुम्-मारने के लिए, स्वजनम् -अपने लोगों को, उद्यताः-उद्यत् ।
अनुवाद : आश्चर्य! कितने दुःख की बात है कि राज्यसुख भोग के लोभवश हम अपने इष्ट-बन्धुओं को मारने का इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं।
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ।।४६ ।।
शब्दार्थ : यदि यदि, माम् -मुझे, अप्रतीकारम् - विरोध का भाव न रखने वाला (मुझको), अशस्त्रम् -बिना शस्त्र के, शस्त्रपाणयः- हाथ में शस्त्र ले कर, धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे समरभूमि में, हन्युः- मार डालें, तत्-वह, मेमेरे लिए, क्षेमतरम् - अधिक कल्याणकारी, भवेत् -होगा।
अनुवाद : यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र रण में मुझ अप्रतीकारी (अविरोधी) और निःशस्त्र को मार भी डालें, तो वह भी मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा।
सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ।।४७ ।।
शब्दार्थ : एवम् - इस प्रकार, उक्त्वा-कह कर, अर्जुनः-अर्जुन, संख्ये-रण में, रथोपस्थे-रथ पर, उपाविशत्-बैठ गया, विसृज्य-छोड़ कर, सशरम् - बाण सहित, चापम् - धनुष को, शोकसंविग्नमानसः - शोकसंतप्त मन से ।
सञ्जय ने कहा
अनुवाद : रणक्षेत्र में इस प्रकार कह कर अपने धनुष-बाण को एक ओर रख कर अर्जुन, शोकाकुल मन से रथ के पृष्ठ भाग में बैठ गया।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ।।
।। इति अर्जुनविषादयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ द्वितीयोऽध्यायः
सांख्ययोगः
सञ्जय उवाच
तं तथा कृपयाऽविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ।।१ ।।
शब्दार्थ : तम्-उसे, तथा- इस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम् वशीभूत, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् - अश्रुपूर्ण नेत्रों से और आकुल, विषीदन्तम्-शोकातुर, इदम् - यह, वाक्यम्-वचन, उवाच-कहा, मधुसूदनः- मधुसूदन ने ।
सञ्जय ने कहा
अनुवाद : करुणार्द्र, विषादयुक्त (शोकातुर) और अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन से मधुसूदन (मधु राक्षस का वध करने वाले कृष्ण) ने इस प्रकार कहा ।
श्री भगवानुवाच
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।
अनार्यजुष्टमस्वर्ण्यमकीर्तिकरमर्जुन ।।२।।
शब्दार्थ : कुतः कहाँ से, त्वा-तुम्हें, कश्मलम्-अवसाद (मन की खिन्नता), इदम्-यह , विषमे संकट काल में, समुपस्थितम्-आ गया, अनार्यजुष्टम् - अनार्य द्वारा आचरित, अस्वर्ण्यम् -स्वर्ग में न ले जाने वाला, अकीर्तिकरम् -अपयश देने वाला, अर्जुन-हे अर्जुन ।
अनुवाद : हे अर्जुन, इस संकट काल में तुम्हारे मन में यह अवसाद कहाँ से उत्पन्न हो गया है? न तो यह आर्यजनों का आचरण है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही यश की प्राप्ति कराने वाला है
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ।।३।।
शब्दार्थ : क्लैब्यम् -नपुंसकता, मा स्म गमः मत प्राप्त करो, पार्थ-अर्जुन, न -नहीं, एतत्-यह, त्वयि-तुम्हें, उपपद्यते-उचित, क्षुद्रम् - अधम, हृदयदौर्बल्यम् -हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ-खड़े हो जाओ, परन्तप - हे शत्रुदमन करने वाले।
अनुवाद : (इस समय) हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त होना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। हे शत्रु को संतप्त करने वाले (अर्जुन), हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ।
अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ।।४ ।।
शब्दार्थ : कथम् -कैसे, भीष्मम् - भीष्म को, अहम् -मैं, संख्ये-युद्ध में, द्रोणम् द्रोण को, च-और, मधुसूदन-मधुसूदन, इषुभिः बाणों से, प्रतियोत्स्यामि -विरुद्ध युद्ध करूँगा, पूजाहौँ-आराध्य, अरिसूदन-शत्रु का नाश करने वाले (कृष्ण)।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूँ क्योंकि हे अरिसूदन ! वे दोनों ही मेरे लिए वन्दनीय हैं।
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव
भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ।।५ ।।
शब्दार्थ : गुरून् गुरुजनों को, अहत्वा-न मार कर, हि-निश्चयेन, महानुभावान् -महापुरुषों को, श्रेयः-कल्याणकारी, भोक्तुम् - भोग करना, भैक्ष्यम् -भिक्षा, अपि-भी, इह-यहाँ, लोके-लोक में, हत्वा-मार कर, अर्थकामान् अर्थ (धन) की कामना वाले, तु-निश्चित रूप से, गुरून् - गुरुजनों को, इह -यहाँ, एव-ही, भुञ्जीय-भोगना, भोगान् - भोगों को (सुखों को), रुधिरप्रदिग्धान् रक्तरंजित ।
अनुवाद : इन प्रशस्त वन्दनीय आचार्यों का हनन करने की अपेक्षा तो भिक्षा का अन्न स्वीकार करना निश्चित रूप से श्रेयस्कर है। वित्तैषणावश (ऐश्वर्य भोग की इच्छा से) गुरुजनों का वध कर के इस लोक में भी तो मैं रक्तरंजित भोगों का ही भोग करूँगा।
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविषाम-
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।।६ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, च-और, एतत्-यह, विद्यः- (हम) जानते हैं, कतरत् क्या, नः- हमारे लिए, गरीयः - श्रेष्ठतर, यत्-जो, वा-अथवा, जयेम-हम जीतें, यदि-यदि, वा-अथवा, नः- हमें, जयेयुः वे जीतें, यान् -जिन्हें, एव-ही, हत्वा-मार कर, न-नहीं, जिजीविषामः- जीवित नहीं रहना चाहते, ते-वे, अवस्थिताः -खड़े हैं, प्रमुखे-समक्ष, धार्तराष्ट्राः- धृतराष्ट्र के पुत्र ।
अनुवाद : हम उन पर विजय प्राप्त करें अथवा वे हमें जीत लें-इन दोनों में श्रेष्ठतर क्या है, हम तो यह भी नहीं जानते। पुनरपि, जिन्हें मारकर हम जीव्रित रहने की अभिलाषा नहीं रखते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे समक्ष खड़े हैं।
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ।।७ ।।
शब्दार्थ : कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः- (भावुकता में) करुणा दोष से अभिभूत स्वभाव वाला, पृच्छामि-पूछता हूँ, त्वाम्-आपको, धर्मसंमूढचेताः कर्तव्य के प्रति भ्रमित चित्त वाला, यत्-जो, श्रेयः-कल्याणकारी, स्यात् -हो, निश्चितम् - निश्चय से, ब्रूहि-कहें, तत्-वह, मे—मेरे लिए, शिष्यः-शिम, ते-आपका, अहम् -मैं, शाधि-शिक्षा दें, माम्-मुझे, त्वाम् आपकी, प्रपन्नम् - शरणागत हूँ।
अनुवाद : मेरा हृदय करुणा रूपी दुर्बलता से ग्रस्त है, कर्तव्य के प्रति मेरा मन भ्रान्त है (मूढ़ है), मैं आपसे पूछता हूँ, निश्चित रूप से जिसमें मेरा कल्याण निहित हो, वही उपदेश मुझे दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ।
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या-
द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ।।८ ।।
शब्दार्थ : न हि-नहीं, प्रपश्यामि-देखता हूँ, मम-मेरा, अपनुद्यात् -दूर करें, यत्-जो, शोकम्-शोक, उच्छोषणम् -सुखाने वाला, इन्द्रियाणाम् - इन्द्रियों को, अवाप्य-प्राप्त करके, भूमौ धरा पर, असपत्नम् -निर्द्वन्द्व, ऋद्धम् -समृद्ध, राज्यम् राज्य, सुराणाम् - देवताओं का, अपि-भी, च-और, आधिपत्यम् स्वामित्व ।
अनुवाद : मैं इस धरा का निर्द्वन्द्व राज्य और देवों पर स्वामित्व भी क्यों न प्राप्त कर लूँ; परन्तु मुझे ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखायी दे रहा, जिससे इन्द्रियों को सुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो सके।
सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप ।
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ।।९।।
शब्दार्थ : एवम् - इस प्रकार, उक्त्वा-कह कर, हृषीकेशम् -कृष्ण को, गुडाकेशः अर्जुन (नींद को जीतने वाला), परन्तप-शत्रु का नाश करने वाला, न-नहीं, योत्स्ये-लडूंगा, इति-ऐसा, गोविन्दम् - गोविन्द को, उक्त्वा-कह कर, तूष्णीम् -मौन, बभूव ह - हो गया।
सञ्जय ने कहा
अनुवाद : हृषीकेश (इन्द्रियों के स्वामी कृष्ण) को परन्तप (शत्रु का नाश करने वाले), गुडाकेश (निद्रा को जीतने वाला) अर्जुन ने इस प्रकार कहा- "हे गोविन्द, मैं युद्ध नहीं करूँगा", और मौन हो गया।
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ।।१० ।।
शब्दार्थ : तम् - उसे, उवाच-कहा, हृषीकेशः - कृष्ण ने, प्रहसन् -हँसते हुए, इव-मानो, भारत-हे भारत, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों, मध्ये मध्य में, विषीदन्तम् -निराश (शोकाकुल), इदम् - यह, वचः- वचन ।
अनुवाद : हे भरतवंशी (धृतराष्ट्र), दोनों सेनाओं के मध्य शोकनिमग्न अर्जुन से भगवान् कृष्ण ने, मानो हँसते हुए, ये शब्द कहे।
श्री भगवानुवाच
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।
गतासूनगतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ।।११ ।।
शब्दार्थ : अशोच्यान् - जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अन्वशोचः-शोक किया, त्वम्-तुमने, प्रज्ञावादान् - ज्ञानपूर्ण वचन, च-और, भाषसे-कहते हो, गतासून् -मृत, अगतासून्-जीवित, च-और, न नहीं, अनुशोचन्ति-शोक करते हैं, पण्डिताः - बुद्धिमान् ।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : तुमने उनके लिए शोक किया जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। पुनरपि, तुम बुद्धिमानों जैसी बातें करते हो । विद्वान् लोग जीवित अथवा मृत के लिए शोक नहीं करते।
व्याख्या : इस श्लोक से गीता-दर्शन प्रारम्भ होता है।
भीष्म और द्रोण के लिए चिन्ता करना उचित नहीं है; क्योंकि वे अपनी वास्तविक प्रकृति से शाश्वत हैं और गुणवान् तथा सच्चरित्र हैं। यद्यपि तुम पाण्डित्यपूर्ण वचन बोल रहे हो, तथापि तुम अज्ञान में हो; क्योंकि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो, जो नित्य होने के कारण शोक करने योग्य नहीं हैं। आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति ही विद्वान् कहलाते हैं। वे मृत अथवा जीवित व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते; क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अजन्मा है। वे यह भी जानते हैं कि मृत्यु का तो अस्तित्व ही नहीं है; क्योंकि सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से पृथक् होना ही मृत्यु कहलाता है। पंचभूतों से निर्मित शरीर से पदार्थों का विश्लेषण और पंचतत्त्वों का अपने मूल स्रोत को जाना ही मृत्यु है। शरीर की परिवर्तनशील प्रकृति और आत्मा की नित्य प्रकृति को अर्जुन भूल गया था। अज्ञानवश वह अपने गुरुजनों और सम्बन्धियों के साथ अपने सम्बन्ध को नित्य मान बैठा था। वह भूल गया था कि वर्तमान जीवन के यह जागतिक सम्बन्ध पूर्वकृत् कर्मों के परिणाम स्वरूप थे। इन कर्मों के क्षय होने पर सभी सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं और दूसरा शरीर धारण करने पर नये कर्म अंकुरित होते हैं।
पूर्वकृत् कार्य कर्म कहलाता है और कर्म के जिस भाग ने वर्तमान अवतरण को जन्म दिया, वह प्रारब्ध कर्म कहा जाता है।
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ।।१२।।
शब्दार्थ : न-नहीं, तु-निश्चित रूप से, एव-ही, अहम् मैं, जातु-किसी काल में, न-नहीं, आसम्-था, न नहीं, त्वम्-तुम, ननहीं, इमे-ये, जनाधिपाः-शासक (राजा), न-नहीं, च-और, एव-ही, ननहीं, भविष्यामः- होंगे, सर्वे-सब, वयम् -हम, अतः- अब से आगे, परम् बाद में।
अनुवाद : ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे अथवा ये राजा नहीं थे और ऐसा समय भी नहीं आयेगा, जब हम सब पुनः नहीं होंगे।
व्याख्या : यहाँ भगवान् कृष्ण आत्मा की अमरता अथवा आत्मा की नित्य प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में आत्मा का अस्तित्व रहता है। भौतिक शरीर को त्यागने के उपरान्त भी मनुष्य की सत्ता रहती है। इससे परे भी जीवन है।
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।।१३ ।।
शब्दार्थ : देहिनः देहधारी (आत्मा) का, अस्मिन् - इसमें, यथा-जैसे, देहे शरीर में, कौमारम् -कुमारावस्था (बाल्यावस्था), यौवनम् - यौवन, जरा-वृद्धावस्था, तथा-वैसे ही, देहान्तरप्राप्तिः अन्य शरीर की प्राप्ति, धीरः- धैर्यवान्, तत्र-उस पर, न-नहीं, मुह्यति-शोक करता है।
अनुवाद : जिस प्रकार से जीवात्मा इस शरीर से कुमार, यौवन और वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, उसी प्रकार से (परिवर्तन क्रम में) नव-देह की प्राप्ति करता है। धीर पुरुष इस पर मोह नहीं करते।
व्याख्या : इस शरीर में जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था आने में कोई बाधा नहीं आती, वैसे ही 'अहम्' के सातत्य में मृत्यु से कोई बाधा नहीं पड़ती। बाल्यावस्था के अवसान (समाप्ति) काल में आत्मा मृत नहीं हो जाता। निश्चित रूप से, ऐसा भी नहीं कि युवावस्था में इसका पुनर्जन्म होता हो। जिस प्रकार से आत्मा बाल्यकाल से युवा और युवा से वृद्धावस्था पर्यन्त अपरिवर्तित रूप से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से एक से दूसरे शरीर में स्थानान्तरण भी अपरिवर्तित रूप से होता है। अतः बुद्धिमान् इसके लिए शोक नहीं करता।
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ।।१४ ।।
शब्दार्थ : मात्रास्पर्शाः- इन्द्रिय-विषय-संयोग, तु-निश्चयेन, कौन्तेय-हे अर्जुन, शीतोष्णसुखदुःखदाः-सरदी, गरमी और सुख-दुःख देने वाले, आगमापायिनः आने-जाने वाले (जिनका आदि भी है और अन्त भी), अनित्याः- अनित्य (क्षणभङ्गुर), तान् - उन्हें, तितिक्षस्व-सहन करो, भारत-हे भारत !
अनुवाद : हे कुन्तीपुत्र, इन्द्रिय-विषयों के संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील तथा अनित्य हैं और सरदी-गरमी एवं सुख-दुःख के देने वाले हैं। इन्हें सहन करो।
व्याख्या : शीत एक काल में सुखद है, तो दूसरे काल में दुःखद । उष्णता शीतकाल में सुखद है; किन्तु ग्रीष्मर्तु में दुःखद । वही विषय एक समय में सुख प्रदान करता है और दूसरे समय में दुःखद हो जाता है। इसलिए सुख-दुःख और सरदी-गरमी देने वाले इन्द्रिय-संयोग तो बनते-बिगड़ते रहते हैं। अतः वे प्रकृति से ही अनित्य हैं। विषयों का सम्बन्ध नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा आदि इन्द्रियों से होता है और (इनसे प्राप्त) प्रत्यक्ष ज्ञान (sensations), शिराओं द्वारा मन तक पहुँचाया जाता है जिसका स्थान मस्तिष्क अथवा बुद्धि में है। सुख-दुःख की अनुभूति मन को होती है। सुख-दुःख और शीत-उष्णता को सहन कर के मनुष्य को मन की सन्तुलित अवस्था का विकास करना चाहिए। (निरूपण-V.22)
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।।१५ ।।
शब्दार्थ : यम्-जिसको, हि-निश्चित रूप से, न व्यथयन्ति - विचलित सः वह, नहीं करते, एते-ये, पुरुषम् -मनुष्य को, पुरुषर्षभ-हे पुरुषश्रेठ, समदुःखसुखम् -सुख-दुःख में समान, धीरम् - धीर पुरुष को, अमृतत्वाय-अमृतत्व के लिए, कल्पते-योग्य है।
अनुवाद : हे पुरुषश्रेष्ठ (अर्जुन), जिस धीर पुरुष को सुख और दुःख विचलित नहीं करते, वही निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी है।
व्याख्या : देहाध्यास अथवा आत्मा का शरीर के साथ एकत्व ही सुख-दुःख का हेतु है। सर्वव्यापक अमृत स्वरूप आत्मा तत्त्व से अभिन्नता स्थापित करने पर मनुष्य सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से मुक्त हो जाता है (उनसे प्रभावित नहीं होता) ।
तितिक्षा अथवा सहनशीलता से आत्मशक्ति का विकास होता है। सुख-दुःख अथवा शीत-उष्म (ताप) को शान्त भाव से सहन करना ज्ञान-मार्ग के साधक के लक्षण हैं। यह षट्सम्पत् में से एक है। यह सम्यक्-ज्ञान की अवस्था है। तितिक्षा स्वयं में तो मोक्षप्रद नहीं है; किन्तु विवेक और अनासक्ति के संयोग से यह आत्म-ज्ञान अथवा अमृतत्व प्रदान करने का कारण बन जाती है। (निरूपण –XVIII.53)
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।।१६ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, असतः-असत् का, विद्यते-है, भावः - अस्तित्व, न-नहीं, अभावः अभाव, विद्यते-है, सतः-सत् का, उभयोः दोनों का, अपि-भी, दृष्टः देखा गया, अन्तः- अन्तिम सत्य, तु-निश्चय से, अनयोः इन दोनों का, तत्त्वदर्शिभिः सत्य का दर्शन करने वालों के द्वारा।
अनुवाद : असत् का अस्तित्व नहीं है और सत् का अभाव नहीं है। दोनों की वास्तविकता तत्त्वदर्शियों (ज्ञानियों) द्वारा देखी गयी है।
व्याख्या : अपरिवर्तनशील एक-रस आत्मा नित्य वर्तमान है। सार-रूप में सत्य केवल यही है। नाम-रूप का यह क्षणिक जगत् नित्य परिवर्तशील है। अतः असत्य है। जीवन्मुक्त इस संसार रूप मृग-मरीचिका और आत्मा की शाश्वत सत्ता के प्रति सदा जागरूक रहता है। अपने ज्ञान-चक्षुओं से वह आत्मा का प्रत्यक्ष-ज्ञान करता है। रज्जु रूपी सत्य का ज्ञान होने पर रज्जु में सर्प की भाँति यह संसार उसके लिए विलुप्त हो जाता है। सब नाम-रूपों में अब वह अन्तर्निहित सार-तत्त्व का दर्शन करता है अर्थात् अस्ति-भाति-प्रिय अथवा सत्-चित्-आनन्द (सच्चिदानन्द) को ही सर्वत्र देखता है। इसीलिए उसे तत्त्वदर्शी अथवा सत्य का ज्ञाता कहा जाता है।
परिवर्तनशील पदार्थ अनित्य हैं और सदा सम रस नित्य हैं।
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति ।।१७ ।।
शब्दार्थ : अविनाशि-विनाश रहित, तु-निश्चयेन, तत्-उसे, विद्धि- जानो, येन-जिसके द्वारा, सर्वम्-समस्त, इदम् - यह, ततम्-व्याप्त, विनाशम् -विनाश, अव्ययस्य अस्य-इस अविनाशी का, न-नहीं, कश्चित्-कोई, कर्तुम् -करने के लिए, अर्हति-समर्थ है।
अनुवाद : जिससे यह सारा (जगत्) व्याप्त है, केवल उसे ही तुम विनाश रहित जानो। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है।
व्याख्या : ब्रह्मन् अथवा आत्मन् आकाश की भाँति सर्वत्र सभी पदार्थों में व्याप्त है। पात्र को यदि तोड़ दिया जाये, तो उसके भीतर अथवा बाहर के आकाश का विनाश करना असम्भव है। इसी भाँति सभी पदार्थ अथवा शरीर नष्ट भी हो जायें, तब भी उनमें व्याप्त ब्रह्मन् अथवा आत्मन् को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह जीवन्त सत्य है-सत् ।
ब्रह्मन् के खण्ड नहीं हो सकते। वह न्यूनाधिक नहीं हो सकता । सम्पत्ति क्षय हो जाने पर लोग गतश्रीक (बरबाद) हो जाते हैं। परन्तु ब्रह्मन् के विषय में ऐसा कुछ नहीं होता, वह तो अव्यय है, क्षय रहित है। इसलिए आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह नित्य विद्यमान है। सर्वदा पूर्ण है। आप्तकाम है। पूर्ण सत् है। अनिर्वचनीय है।
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ।।१८ ।।
शब्दार्थ : अन्तवन्तः नश्वर, इमे-ये, देहाः-शरीर, नित्यस्य - शाश्वत के, उक्ताः-कहे गये हैं, शरीरिण:-जीवात्मा के, अनाशिनः अविनाशी के, अप्रमेयस्य-परिमाण रहित, तस्मात् - इसलिए, युध्यस्व-युद्ध करो, भारत- है भारत ।
अनुवाद : नित्य, अविनाशी, अप्रमेय शरीरधारी जीवात्मा के ये शरीर नश्वर हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो।
व्याख्या : भगवान् कृष्ण अर्जुन को सर्वव्याप्त, शाश्वत आत्मा की प्रकृति को अनेक प्रकार से समझाते हुए उसके अज्ञान से उत्पन्न शोक, मोह और भ्रम को दूर करते हुए उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं।
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।।१९ ।।
शब्दार्थ : यः जो, एनम्-इसे, वेत्ति-जानता है, हन्तारम् - मारने वाला, यः जो, चऔर, एनम्-इसे, मन्यते-मानता है, हतम् - मरा हुआ, उभौ वे दोनों, तौ वे दोनों, ननहीं, विजानीतः- जानते, न नहीं, अयम्-यह, हन्ति-मारता है, न-नहीं, हन्यते - मारा जाता है।
अनुवाद : जो व्यक्ति इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मृत समझता है, वे दोनों इसे नहीं जानते; क्योंकि जीवात्मा न तो मारता है, न ही मरता है।
व्याख्या : जीवात्मा अकर्ता है, निर्विकार है। मरने के कर्म का न तो यह हेतु (कर्ता) है और न ही विषय । देहाध्यास अथवा अहं के कारण जो स्वयं को 'मारने वाला' अथवा 'मृत' समझता है, वह वास्तव में आत्मा की वास्तविक प्रकृति से अनभिज्ञ है। आत्मा अविनाशी है। यह तीनों कालों में विद्यमान है। यह सत् (Existence) है। शरीर का विनाश होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता। किसी भी अवस्था में शरीर तो परिवर्तनशील है। इसे (आत्मा को) तो दूसरा शरीर धारण करना है। यह अनिवार्य सत्य है। किन्तु आत्मतत्त्व इससे प्रभावित नहीं होता। श्लोक १९, २०, २१, २३ और २४ आत्मा की नित्यता का वर्णन करते हैं। (निरूपण-XVIII.17)
न जायते प्रियते वा कदाचि-
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।।२० ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, जायते-जन्म लेता है, म्रियते-मरता है, वा-अथवा, कदाचित् कभी भी, न-नहीं, अयम्-यह (आत्मा), भूत्वा हो कर, भविता-होगा, वा-अथवा, ननहीं, भूयः पुनः, अजः- जन्म रहित, नित्यः- शाश्वत, शाश्वतः - अपरिवर्तनशील, अयम्-यह, पुराणः- पुरातन, न नहीं, हन्यते-मारा जाता है, हन्यमाने-मारा जाने पर, शरीरे-शरीर में।
अनुवाद : जन्म-मरण से रहित यह आत्मा न तो कभी जन्म लेता और न ही कभी मरता है। ऐसा भी नहीं कि एक बार उत्पन्न हो कर इसका पुनः अस्तित्व न होगा। यह तो अजन्मा, अनादि, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरता ।
व्याख्या : यह आत्मा जन्म, भाव (अस्तित्व), विकास, परिवर्तन, क्षय और मृत्यु, इन छह भाव-विकारों से शून्य है। अखण्ड होने के कारण यह परिमाण में लघु नहीं होता। न यह बढ़ता है, न घटता है। यह सदा सम रहता है। जन्म-मृत्यु तो भौतिक शरीर के ही गुण हैं। सर्वव्यापक शाश्वत आत्मा का तो जन्म और मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकते ।
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ।।२१ ।।
शब्दार्थ : वेद-जानता है, अविनाशिनम् - विनाश रहित को, नित्यम् - शाश्वत, यः जो, एनम्-इसको, अजम् - जन्म रहित, अव्ययम् - अपरिवर्तनशील, कथम् -कैसे, सः-वह, पुरुषः- मनुष्य, पार्थ-अर्जुन, कम् - किसे, घातयति-मरवाता है, हन्ति-मारता है, कम् - किसे ।
अनुवाद : जो मनुष्य इसे विनाश रहित, नित्य, अजन्मा और निर्विकारी मानता है, वह मनुष्य हे अर्जुन, कैसे किसी को मरवा सकता है अथवा मार सकता है?
व्याख्या : ज्ञानोद्दीप्त साधु प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा आध्यात्मिक अनुभव द्वारा अविकारी, अविनाशी आत्मा का बोध कर लेता है। वह न तो मारने का कर्म कर सकता है और न ही मरवा सकता है।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।।२२ ।।
शब्दार्थ : वासांसि-वस्त्र, जीर्णानि-जीर्ण-शीर्ण (फटे-पुराने), यथा-जैसे, विहाय-त्याग कर, नवानि-नये, गृह्णाति-धारण करता है, नरः मनुष्य, अपराणि-अन्य, तथा-वैसे, शरीराणि-शरीर, विहाय-त्याग कर, जीर्णानि-पुराने, अन्यानि-अन्य, संयाति-धारण करता है, नवानि-नये, देही-देहधारी आत्मा ।
अनुवाद : जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जीर्ण-शीर्ण वस्त्रों को उतार कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह देहधारी आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।।२३ ।।
शब्दार्थ : न -नहीं, एनम् -इसे (आत्मा को), छिन्दन्ति-काट सकते हैं, शस्त्राणि-शस्त्र, न-नहीं, एनम्-इसे, दहति-जलाता है, पावकः- अग्नि,न-नहीं, च-और, एनम्-इसे, क्लेदयन्ति-भिगो सकता है, आपः- जल, न-नहीं, शोषयति-सुखा सकता है, मारुतः - वायु ।
अनुवाद : शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता।
व्याख्या : आत्मा अखण्ड है। इसके खण्ड नहीं हैं। यह अतीव सूक्ष्म है। यह अनन्त है, अतः तलवार इसे काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता।
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।।२४ ।।
शब्दार्थ : अच्छेद्यःन कटने वाला (जिसे छेदा न जा सके), अयम् - यह (आत्मा), अदाह्यः- जिसे जलाया न जा सके, अयम्-यह, अक्लेद्यः गीला न किया जा सके, अशोष्यः सुखाया न जा सके, एव-ही, च- और, नित्यः-नित्य, सर्वगतः सर्वव्यापक, स्थाणुः-अपरिवर्तनशील, अचलः-अचल (गतिहीन), अयम्-यह, सनातनः शाश्वत ।
अनुवाद : न तो यह आत्मा कटने योग्य है, न इसे जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है और न ही इसे सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्याप्त, स्थिर, अचल और शाश्वत है।
व्याख्या : आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म है। यह मन और वाणी की पहुँच (उपगमन) से परे है। इस सूक्ष्म आत्मा का बोध अतीव दुष्कर है। अमर आत्मा की प्रकृति का व्याख्यान और विश्लेषण भगवान् कृष्ण अनेक प्रकार के दृष्टान्तों से करते हैं, ताकि समान्य जन इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें।
इस आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, अतः यह शाश्वत है। क्योंकि यह शाश्वत है, इसलिए यह सर्वव्यापक भी है। सर्वव्यापक होने के कारण यह मूर्तिवत् स्थिर है। स्थिर है, इसलिए अचल है। अचल है, इसी कारण नित्य विद्यमान है। इसीलिए इसका कोई कारण नहीं है (यह स्वयंभू है)। नवीन भी नहीं है। यह सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है।
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ।। २५ ।।
शब्दार्थ : अव्यक्तः- अप्रकट, अयम् - यह (आत्मा), अचिन्त्यः - कल्पनातीत, अयम् - यह, अविकार्यः - अपरिवर्तनशील, अयम् - यह, उच्यते- कहा जाता है, तस्मात् - इसलिए, एवम् - इस प्रकार, विदित्वा-जान कर, एनम् इसको, ननहीं, अनुशोचितुम् - शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो ।
अनुवाद : यह आत्मा अव्यक्त है, अचिन्त्य और अविकारी है। इस प्रकार से इसे जान कर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
व्याख्या : आत्मा दृग्विषय (दृष्टि का विषय) नहीं है। भौतिक चक्षु से इसका दर्शन असम्भव है। अतः यह आत्मा अप्रकट है। नेत्रों से दर्शनीय विषय चिन्तन का विषय बन जाता है; किन्तु इसे नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। अतः यह अचिन्त्य है। दूध को छाछ में मिला दिया जाये, तो उसका स्वरूप परिवर्तित हो जायेगा। किन्तु दुग्ध की भाँति इस आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता । इसीलिए यह अविकारी और अपरिवर्तनशील है। अतः इस प्रकार से आत्मा को समझ कर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वह भी तुम्हारे लिए सोचना उचित नहीं कि तुम उनको मारने वाले हो और वे तुम्हारे द्वारा मारे गये हैं।
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ।। २६ ।।
शब्दार्थ : अथ-अब, च-और, एनम्- इसे (आत्मा को), नित्यजातम् - नित्य जन्म लेने वाला, नित्यम्-सदा, वा-यदि, मन्यसे मानते हो, मृतम्-मरा हुआ, तथापि-फिर भी, त्वम्-तुम, महाबाहो -शूरवीर, न-नहीं, एवम् - इस प्रकार, शोचितुम्-शोक के लिए, अर्हसि-योग्य हो ।
अनुवाद : पुनरपि, हे अर्जुन, यदि तुम इसे नित्य जन्म लेने और मरने वाला समझते हो, तब भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है।
व्याख्या : तर्क के लिए भगवान् कृष्ण यहाँ लोकप्रिय सम्भावना का आलम्बन लेते हैं। मान लो, शरीर के अस्तित्व में आने पर आत्मा पुनः-पुनः जन्म लेता है और शरीर के मरने पर पुनः-पुनः मरता है, तथापि हे महाबाहो (शूरवीर अर्जुन), तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए; क्योंकि मृतक के लिए जन्म लेना अनिवार्य है और जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु अपरिहार्य है। यह सृष्टि का अटल एवं कठोर नियम है।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ।।२७ ।।
शब्दार्थ : जातस्य-जन्म लेने वाले की, हि-निश्चित रूप से, ध्रुवः-निश्चित, मृत्युः मृत्यु, ध्रुवम् -निश्चित, जन्म-जन्म, मृतस्य-मृत का, च-और, तस्मात् - इसलिए, अपरिहार्ये-जो टल न सके, अर्थ-के लिए, न-नहीं, त्वम् -तुम, शोचितुम्-शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो।
अनुवाद : जन्म लेने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है और मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है। जिसका कोई निराकरण ही नहीं है अर्थात् जो बात टल नहीं सकती, उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
व्याख्या : मृत का जन्म निश्चित और जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। जन्म और मृत्यु तो अपरिहार्य (अटल) है। अतः अपरिहार्य के लिए शोक उचित नहीं ।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।।२८ ।।
शब्दार्थ : अव्यक्तादीनि-जन्म से पूर्व अप्रकट, भूतानि-समस्त प्राणी, व्यक्तमध्यानि-मध्य में प्रकट, भारत-हे अर्जुन, अव्यक्तनिधनानि-अन्त में भी अप्रकट, एव-ही, तत्र-वहाँ, का-क्या, परिदेवना-शोक ।
अनुवाद : समस्त प्राणी (सृष्टि के) आदि में अप्रकट रहते हैं और मध्य में प्रकट रूप में होते हैं। अन्त में हे अर्जुन, पुनः अप्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से शोक करने का कोई कारण ही नहीं है।
व्याख्या : भौतिक शरीर पंचतत्त्वों का संघात (संयोग) है। पंचतत्त्वों का एवंविध संघात होने पर ही यह भौतिक नेत्रों द्वारा दर्शनीय है। मृत्यूपरान्त शरीर के पंचतत्त्व विघटित हो जाते हैं और अपने-अपने मूल स्रोत की ओर उपगमन करते हैं। तब यह अदृश्य होता है। अतः मध्य काल में शरीर दृष्टिगोचर हो जाता है। मोहवश ही पुत्र, मित्र, आचार्य, पिता, माता, पत्नी, भ्राता और स्वसा (बहन) आदि सम्बन्ध बनते हैं। जिस प्रकार एक नदी में शिलाखण्ड मिलते और बिछुड़ते रहते हैं, इसी प्रकार माता-पिता, पुत्र और बन्धुजनों का इस संसार में संयोग-वियोग होता रहता है। यह संसार तो एक बहुत बड़ा पथिकाश्रम है। पथिकों का संयोग-वियोग तो यहाँ होता रहता है।
प्रारम्भ और अन्त में पात्र की सत्ता नहीं होती । प्रारम्भ और अन्त में देखने पर विचार करना चाहिए कि यह पात्र तो मात्र भ्रान्ति है, इसका अस्तित्व क्षणिक है। एवंविध आदि और अन्त में शरीरों का अस्तित्व नहीं होता और जो आदि और अन्त में नहीं है, मध्य में भी वह भ्रम हो सकता है। विचार कर के अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए कि वस्तुतः मध्य में भी शरीर का अस्तित्व नहीं है।
शरीर की इस प्रकृति और इस पर आधारित सभी सम्बन्धों को समझने वाला व्यक्ति शोक नहीं करेगा।
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन-
माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः ।
आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ।।२९ ।।
शब्दार्थ : आश्चर्यवत् - आश्चर्य की भाँति, पश्यति-देखता है, कश्चित् -कोई, एनम् - इसे (आत्मा को), आश्चर्यवत्-आश्चर्य की भाँति, वदति-बोलता है, तथा-वैसे, एव-ही, च-और, अन्यः- अन्य, आश्चर्यवत् - आश्चर्य की भाँति, च-और, एनम्-इसे, अन्यः - अन्य, शृणोति-सुनता है, श्रुत्वा-सुन कर, अपि-भी, एनम्-इसे, वेद-जानता है, न-नहीं, च-और, एव-ही, कश्चित् -कोई।
अनुवाद : इस आत्मा को कोई (पुरुष) तो आश्चर्य की भाँति देखता है, अन्य इसके लिए आश्चर्य की भाँति वचन कहता है, कोई और आश्चर्य की भाँति इसका श्रवण करता है और श्रवण कर के भी इसे कोई समझ नहीं पाता ।
व्याख्या : इस श्लोक की विवेचना इस प्रकार भी की जा सकती है। जो इस आत्मा का दर्शन, वाचन और श्रवण करता है, वह अद्भुत व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति विरल ही होता है। सहस्रों में कोई एक ही ऐसी निष्ठा वाला होता है। अतः उचित ही कहा है कि आत्मा को समझना अत्यन्त दुष्कर है।
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ।। ३० ।।
शब्दार्थ : देही-अन्तर्निवसित (आत्मा), नित्यम् सदा, अवध्यः- अवध्य (जिसे मारा न जा सके), अयम्-यह, देहे-शरीर में, सर्वस्य-सबके, भारत-हे भारत, तस्मात्-इसलिए, सर्वाणि-समस्त, भूतानि-प्राणी, न-नहीं, त्वम् -तुम, शोचितुम् - शोक करने के लिए, अर्हसि -योग्य हो ।
अनुवाद : प्रत्येक प्राणी का अन्तःस्थ आत्मा नित्य अवध्य है; इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
व्याख्या : किसी भी प्राणी का शरीर तो नष्ट हो सकता है; पर आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। अतः तुम्हें किसी के लिए भी शोक नहीं करना है, चाहे वे भीष्मपितामह हों अथवा कोई अन्य भी क्यों न हो।
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।
धर्माद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ।। ३१ ।।
शब्दार्थ : स्वधर्मम् - अपने कर्तव्य को, अपि भी, च-और, अवेक्ष्य-देख कर, न-नहीं, विकम्पितुम् - विचलित होना, अर्हसि चाहिए, धर्मात् -धर्म से, हि-निश्चय से, युद्धात् - युद्ध की अपेक्षा से, श्रेयः-कल्याणप्रद, अन्यत् अन्य, क्षत्रियस्य-क्षत्रिय का, न विद्यते-नहीं है।
अनुवाद : अपने कर्तव्य को देखते हुए भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़ कर कोई और श्रेष्ठतर कार्य नहीं है।
व्याख्या : अब भगवान् कृष्ण अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने के लिए सांसारिक तर्क देते हैं। अभी तक तो भगवान् कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के विषय में उपदेश करते हुए उसे दार्शनिक तर्क दे रहे थे। अब वे अर्जुन से कहते हैं-"हे अर्जुन, युद्ध तो क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य है। उस कर्तव्य से तुम्हें विमुख नहीं होना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़ कर और कुछ भी प्रशस्य नहीं है। योद्धा को तो (युद्ध में) लड़ना ही शोभा देता है।
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ।। ३२ ।।
शब्दार्थ : यदृच्छया-स्वेच्छया (स्वयं ही), च-और, उपपन्नम् - प्राप्त हुए, स्वर्गद्वारम् स्वर्गलोक का द्वार, अपावृतम्-खुला हुआ, सुखिनः सुखी, क्षत्रियाः-क्षत्रिय लोग, पार्थ-हे अर्जुन, लभन्ते-प्राप्त करते हैं, युद्धम् - युद्ध, ईदृशम् - इस प्रकार का ।
अनुवाद : हे अर्जुन, स्वर्ग लोक के खुले द्वार की भाँति स्वयं-प्राप्त युद्ध के इस प्रकार के संयोग को प्राप्त कर क्षत्रिय धन्य हो जाते हैं।
व्याख्या : शास्त्र का कथन है कि यदि कोई क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता हुआ प्राण त्याग देता है, तो सद्यः स्वर्ग को प्राप्त करता है।
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ।
ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।। ३३ ।।
शब्दार्थ : अथ-अतः, चेत्-यदि, त्वम्-तुम, इमम् -इस, धर्म्यम् - धर्म के, संग्रामम् - युद्ध को, न-नहीं, करिष्यसि करोगे, ततः-तब, स्वधर्मम् - अपने कर्तव्य को, कीर्तिम्-यश को, च-और, हित्वा-खो कर, पापम् -पाप को, अवाप्स्यसि-प्राप्त करोगे ।
अनुवाद : किन्तु यदि तुम इस धर्मयुद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो अपने कर्तव्य और यश से च्युत हो कर पाप के भागी बनोगे ।
व्याख्या : भगवान् कृष्ण अर्जुन को उसके द्वारा अर्जित कीर्ति का स्मरण कराते हुए कह रहे हैं कि यदि इस समय वह युद्ध नहीं करेगा, तो कीर्ति खो देगा । भगवान् शिव से युद्ध कर के अर्जुन ने यश पाया था। एक बार अर्जुन यात्रा के लिए हिमालय की ओर बढ़ा। पर्वतारोही (किरात) के रूप में आये भगवान् शिव से उसने युद्ध किया और उनसे स्वर्गीय दिव्यास्त्र 'पशुपतास्त्र' प्राप्त किया।
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ।। ३४ ।।
शब्दार्थ : अकीर्तिम् -अपयश, च-और, अपि-भी, भूतानि सब लोग, कथयिष्यन्ति-कहेंगे, ते-तेरे लिए, अव्ययाम् -सदा के लिए, सम्भावितस्य-यशस्वी का, च-और, अकीर्तिः-अपयश, मरणात् मरने से, अतिरिच्यते-बढ़ कर है।
अनुवाद : चिरकाल पर्यन्त सभी लोग तेरे अपयश का वर्णन करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़ कर है।
व्याख्या : संसार भी तेरी अकीर्ति का स्मरण कर तुम्हें सदा (स्मृतियों में) जीवित रखेगा। एक सम्मानित शूरवीर और सद्गुणों से युक्त महान् योद्धा के लिए अपमानित जीवन जीने से तो मृत्यु अधिक श्रेयस्कर है।
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ।। ३५ ।।
शब्दार्थ : भयात् - भय से, रणात् - युद्धक्षेत्र से, उपरतम् -विमुख, मंस्यन्ते-मानेंगे, त्वाम् - तुम्हें, महारथाः- महान् योद्धा, येषाम् - जिनके लिए, च-और, त्वम् तुम, बहुमतः आदरणीय, भूत्वा-हो कर, यास्यसि-पाओगे, लाघवम् लघुता को।
अनुवाद : महान् योद्धा सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से विमुख हो गये हो। जिनके लिए तुम आदर के योग्य थे, वही योद्धा अब तुम्हें क्षुद्र समझेंगे ।
व्याख्या : दुर्योधन तथा अन्य योद्धा निश्चित रूप से यही सोचेंगे कि तुम कर्ण तथा अन्य वीरों के भय से युद्ध से भागे हो। गुरु जनों के प्रति आदर और दया के भाव से तुम युद्ध से विमुख हो रहे हो, ऐसा वे नहीं सोच सकते । तुम्हारे पौरुष, शौर्य और अन्य सद्गुणों के कारण दुर्योधन सहित अन्य योद्धाओं ने जो तुम्हें सम्मान दिया है, वह लघुता को प्राप्त होगा; क्योंकि वे तुम्हें रण से भागने के कारण तुच्छ समझ कर तुम्हारा अपमान करेंगे।
अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम् ।। ३६ ।।
शब्दार्थ : अवाच्यवादान् -कटु शब्द, च-और, बहून् बहुत, वदिष्यन्ति-बोलेंगे, तव-तुम्हारे, अहिताः-शत्रु, निन्दन्तः - निन्दा करते हुए, तव-तुम्हारे, सामर्थ्यम् -शक्ति, ततः- उसकी अपेक्षा, दुःखतरम् - अधिक दुःखद, नु-निश्चित रूप से, किम्-क्या है।
अनुवाद : तुम्हारे शत्रु भी अनेक प्रकार से तुम्हारी क्षमता की निन्दा करते हुए कटु वचन कहेंगे। इससे और अधिक दुःखद स्थिति क्या हो सकती है?
व्याख्या : वास्तव में ऐसे अपभाषण की अपेक्षा कोई और कष्ट इतना असह्य और वेदनाशील नहीं हो सकता।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।। ३७ ।।
शब्दार्थ : हतः मारा जाने पर, वा-अथवा, प्राप्स्यसि-प्राप्त करोगे, स्वर्गम् -स्वर्ग को, जित्वा-जीत कर, वा-अथवा, भोक्ष्यसे-भोगोगे, महीम् - पृथ्वी को, तस्मात् - इसलिए, उत्तिष्ठ-उठो, कौन्तेय-कुन्तीपुत्र, युद्धाय-युद्ध के लिए, कृतनिश्चयः - निश्चय कर के।
अनुवाद : मारे जाने पर स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे और विजय प्राप्त करने पर धरती का राज्य भोगोगे। अतः हे कुन्तीपुत्र, उठो, युद्ध के लिए संकल्प करो।
व्याख्या : किसी भी अवस्था में हित तो तुम्हारा ही होगा। इसलिए दृढ़संकल्प के साथ खड़े हो जाओ -"या तो मैं शत्रु को जीत लूँगा, अन्यथा (लड़ते हुए) प्राण त्याग दूँगा।"
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।। ३८ ।।
शब्दार्थ : सुखदुःखे-सुख और दुःख में, समे-समभाव, कृत्वा कर के (रह कर), लाभालाभौ-लाभ और हानि में, जयाजयौ-जीत और हार में, ततः-तत्पश्चात्, युद्धाय-युद्ध के लिए, युज्यस्व-संलग्न हो जाओ, ननहीं, एवम् - इस प्रकार, पापम् -पाप को, अवाप्स्यसि-प्राप्त करोगे ।
अनुवाद : सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय में समभाव रह कर अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा।
व्याख्या : यह समता योग अथवा कर्म समीकरण (समचित्तभाव) का सिद्धान्त है। मन की साम्यावस्था में कर्म करने से मनुष्य उसके फल का भागी नहीं बनता। ऐसा कर्म जो मनोभावों से ऊपर रह कर अर्थात् भावुकतापूर्ण उतार-चढ़ावों से पृथक् रह कर किया जाता है, मन-हृदय को पवित्र करता है और भवबन्धन से मुक्त करने वाला होता है। जागृत प्रयासों और सतत संघर्ष के द्वारा मन की इस साम्यावस्था को विकसित किया जा सकता है।
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।
बुद्धयायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।।३९ ।।
शब्दार्थ : एषा यह, ते तुम्हारे लिए, अभिहिता-कही गयी, सांख्ये सांख्य में, बुद्धिः ज्ञान, योगे-योग में, तु-निश्चय से, इमाम् इसको, शृणु-सुनो, बुद्धया बुद्धि से, युक्तः - युक्त हो कर, यया-जिससे, पार्थ-हे पार्थ, कर्मबन्धम् -कर्म के बन्धन को, प्रहास्यसि -त्याग दोगे।
अनुवाद : हे अर्जुन, अभी मैंने सांख्य का ज्ञान तुम्हें दिया है। अब योग के विषय में सुनो, जिस ज्ञान का श्रवण कर तुम कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाओगे।
व्याख्या : अब तक भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया (सांख्य योग, वेदान्त अथवा ज्ञानयोग का मार्ग है जो विधानों को और आत्म-साक्षात्कार के अन्य विधि-विधानों को प्रशस्त करता है। यह कपिल मुनि का सांख्य योग नहीं है) । अब वे अर्जुन को कर्मयोग का रहस्य बताने लगे हैं, जिसे जान कर वह अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति कर्मबन्धन तोड़ कर मुक्त हो सकता है।
कर्मयोगी को कर्मफल की आशा त्याग कर और कर्ताभाव से ऊपर उठ कर कर्म करना चाहिए। उसका कर्म सभी प्रकार के द्वन्द्वों-जैसे जय-पराजय, हानि-लाभ और सुख-दुःख आदि से परे रह कर आसक्तिभाव से रहित होना चाहिए। अहंभाव से शून्य और अनासक्त रह कर कर्म करने वाले का, धर्म-अधर्म और पाप-पुण्य स्पर्श भी नहीं कर सकते। कर्मयोगी अपने समस्त कर्म ईश्वरार्पण करके ईश्वर-प्रसाद ग्रहण करता है।
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।४० ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, इह-यहाँ (इस योग में), अभिक्रमनाशः - प्रयत्न का विनाश, अस्ति-है, प्रत्यवायः - विपरीत परिणाम की उत्पत्ति, न-नहीं, विद्यते-है, स्वल्पम् -थोड़ा, अपि-भी, अस्य-इस, धर्मस्य कर्तव्य का, त्रायते-रक्षा करता है, महतः महान् (से), भयात् भय से ।
अनुवाद : इस योग में कोई भी प्रयास विफल नहीं होता और न ही कोई बाधा आती है (अर्थात् विपरीत परिणामों की उत्पत्ति अथवा उल्लंघन नहीं होते) । इस ज्ञान का थोड़ा-सा पालन भी महान् भय से रक्षा करता है।
व्याख्या : यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया जाये, तो वह अनुष्ठान व्यर्थ है; क्योंकि कर्ता उसके फल से वंचित रह जाता है। किन्तु कर्मयोग में ऐसा नहीं है; क्योंकि प्रत्येक कर्म हृदय की तत्काल शुद्धि करता है।
कृषि में सन्दिग्धता है। कृषक भूमि जोतेगा, हल चलायेगा, बीज बोयेगा और यदि वर्षा न हो, तो फसल प्राप्त नहीं कर सकता । कर्मयोग में ऐसा नहीं है। अनिश्चितता इसमें कदापि नहीं है। और भी, किसी प्रकार की कोई हानि होने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। औषध-उपचार में चिकित्सक द्वारा अयुक्त औषध मिलने पर विपरीत परिणाम हो सकते हैं; किन्तु कर्मयोग में ऐसा नहीं है। कर्मयोग के इस मार्ग में अल्पमात्र भी किया गया प्रयास जन्म-मृत्यु के महान् बन्धन से छुटकारा दिला सकता है। भगवान् कृष्ण यहाँ अर्जुन में इस योग के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए, उसे इसमें प्रेरित करने के लिए कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं।
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ।।४१ ।।
शब्दार्थ : व्यवसायात्मिका-दृढ़ संकल्प वाली, बुद्धिः बुद्धि, एका-एक, इह-यहाँ, कुरुनन्दन- हे कुरु वंश के प्रिय, बहुशाखाः- अनन्त शाखाओं वाली (विकीर्ण), हि-निश्चित रूप से, अनन्ताः- अनन्त, च-और, बुद्धयः-विचार, अव्यवसायिनाम् -संकल्पशून्य व्यक्तियों के।
अनुवाद : हे कुरुनन्दन, यहाँ (इस कर्मयोग मार्ग में) दृढ़संकल्प बुद्धि एक ही है; किन्तु अनिश्चित (चंचल) मन वालों के विचार विकीर्ण और अनन्त होते हैं।
व्याख्या : इह लोक में, आनन्द सागर में अवगाहन हेतु सुनिश्चित संकल्प एक ही है, वह है एकचित् (अनन्य-मनस्क) संकल्प। यह अद्वितीय विचार ज्ञान के सम्यक् स्रोत से उदित होता है। योग का साधक मन की विकीर्ण रश्मियों (विचारों) को संहत (एकत्र) करता है। एकाग्रता, अनासक्ति और विवेक से वह इन्हें एकस्थ करता है। वह मन की अस्थिर और चंचल वृत्ति से मुक्त होता है।
संसार रूपी पंक में डूबे हुए सांसारिक मनुष्य के पास एकाग्र वृत्ति नहीं होती। वह अनन्त विचारों का सत्कार करता है। उसका मन सदा चंचल और अस्थिर रहता है।
यदि विचार न रहें, तो संसार भी नहीं रहेगा। मन से अगणित विचारों का उद्भव होता है और इसी से संसार अस्तित्व में आता है। विचार, नाम और रूप अभिन्न हैं, इन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता। यदि विचारों को संयत कर लिया जाये, तो मन संयत हो जाता है और योगी मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।।४२ ।।
शब्दार्थ : याम् -जिस, इमाम्-इस, पुष्पिताम् -पुष्पों जैसी आकर्षक, वाचम् वाणी, प्रवदन्ति-कहते हैं, अविपश्चितः- अविवेकी, वेदवादरताः- वेद के कथन में आनन्द लेने वाले, पार्थ- हे अर्जुन, न-नहीं, अन्यत् - अन्य, अस्ति-है, इति-इस प्रकार, वादिनः-कहने वाले ।
अनुवाद : हे अर्जुन, अविवेकी जन वेदों की पुष्पिता (आकर्षक) वाणी बोलते हुए वेदों के गुण-स्तुतिमय वाक्यों में आनन्द लेते हैं और कहते हैं- 'इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है।'
व्याख्या : विवेकशून्य व्यक्ति वेदों के कर्मकाण्ड में अधिक आस्था रखते हैं, जिसमें किसी विशेष फल-प्राप्ति हेतु विशेष विधि-विधानों की कर्मविधि और स्तुति का वर्णन है। स्वर्ग के आनन्द का वर्णन करने वाले इन वेदवाक्यों में वे अत्यधिक अनुरक्त हो जाते हैं। उनके अनुसार कर्मकाण्ड के अनुष्ठानों से प्रापणीय स्वर्गिक सुखों से परे अन्य कुछ भी नहीं है।
वेदों के दो भाग हैं-कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। ब्राह्मण ग्रन्थ और संहिता कर्मकाण्ड से सम्बद्ध हैं। जैमिनी का पूर्व मीमांसा मत इसी पर आधारित है। इस मत के अनुयायी इहलोक के ऐश्वर्य और स्वर्ग-सुख की प्राप्ति हेतु इस प्रकार के अनेक यज्ञादि कर्मों का प्रतिपादन करते हैं। वे इसे ही मनुष्य-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। सामान्य जन तो इसके स्तवन-पाठ से ही आकृष्ट हो जाते हैं। उपनिषद् और आरण्यक ग्रन्थ परब्रह्म की प्रकृति का वर्णन करते हैं और ज्ञान काण्ड के अन्तर्गत हैं।
स्वर्ग का जीवन भी अस्थायी है। पुण्य कर्म क्षीण होने पर मनुष्य को धरालोक पर लौटना पड़ता है। सहस्रों यज्ञ करने पर भी आत्म-ज्ञान के बिना मोक्ष-प्राप्ति असम्भव है।
भगवान् कृष्ण, धरती का प्रभुत्व दिलाने वाले और स्वर्ग तथा अन्य शक्तियाँ प्रदान करने वाले वैदिक अनुष्ठानों के प्रशंसक, मीमांसा सिद्धान्त को अपेक्षाकृत गौण बताते हैं; क्योंकि वे आत्यन्तिक मोक्ष प्रदान करने वाले नहीं हैं।
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।।४३ ।।
शब्दार्थ : कामात्मानः- इच्छाओं से पूर्ण, स्वर्गपराः-स्वर्ग-प्राप्ति ही जिनका लक्ष्य हो, जन्मकर्मफलप्रदाम् -कर्मों के परिणामस्वरूप नव-जन्म की ओर ले जाने वाला, क्रियाविशेषबहुलाम् - विविध प्रकार की प्रचुर क्रियाएँ, भोगैश्वर्यगतिं प्रति-इन्द्रियतुष्टि, ऐश्वर्य और स्वामित्व-प्राप्ति के लिए।
अनुवाद : इच्छाओं से पूर्ण, स्वर्ग को अपना आत्यन्तिक लक्ष्य मान कर (वे ऐसी वाणी बोलते हैं जो कर्मफल प्रदान करने वाली है), कर्मों के फलस्वरूप नया जन्म प्रदान करने वाली है। इस प्रकार वे विविध विधियाँ विशेष कर्मकाण्डों में अपनाते हैं जो भौतिक सुख, साम्राज्य और प्रभुत्व देने वाली हैं।
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।।४४ ।।
शब्दार्थ : भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् - इन्द्रिय-सुख और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की, तया-उसके द्वारा, अपहृतचेतसाम् - जिनका चित्त मोहग्रस्त हो गया हो, व्यवसायात्मिका-दृढ़ निश्चय वाली, बुद्धिः - बुद्धि, समाधौ-समाधि में, न-नहीं, विधीयते-स्थिर रहती है।
अनुवाद : (वेद की) इस शिक्षा के द्वारा जो लोग सांसारिक भोगों में आसक्त हो कर मोहग्रस्त हो गये हैं, उनकी निश्चयात्मिका (भले-बुरे का विवेक करने वाली) बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं हो सकती ।
व्याख्या : प्रभुत्व और सुख-समृद्धि के इच्छुक मन की एकाग्रता नहीं प्राप्त कर सकते। वे एकाग्रचित्त हो कर ध्यान में नहीं बैठ सकते। वे तो अर्थ और सामर्थ्य-प्राप्ति की योजनाएँ बनाते रहते हैं। उनके मन सदा व्याकुल रहते हैं। उनमें तुलनात्मक बुद्धि का अभाव रहता है।
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ।।४५ ।।
शब्दार्थ : त्रैगुण्यविषयाः-तीन गुणों से सम्बन्धित, वेदाः वेद, निखैगुण्यः-तीन गुणों से परे, भव-हो जाओ, अर्जुन-हे अर्जुन, निर्द्वन्द्वः - द्वन्द्वों से परे, नित्यसत्त्वस्थः - नित्य सत्त्व भाव में स्थित रहने वाले, निर्योगक्षेम: लाभ और संचय के भाव से मुक्त, आत्मवान्-आत्मा में स्थित।
अनुवाद : वेद (प्रकृति के) तीन गुणों का वर्णन करते हैं। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। हे अर्जुन, अर्जन (लाभ) और रक्षण (संचित अथवा अर्जित धन की रक्षा) के भाव से तथा द्वन्द्वों से मुक्त हो कर सत्त्व में विचरण करो तथा आत्मस्थ हो जाओ।
व्याख्या : गुण द्रव्य भी हैं और गुण भी। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्त्व गुण शुद्धता, प्रकाश और समन्वय का परिचायक है। रजस्, मोह और गति (क्रियाशीलता) है। तमस् अन्धकार व जड़ता की ओर संकेत करता है। मान-अपमान, आदर-अनादर, जय-पराजय, हानि-लाभ, सुख-दुःख और शीतोष्ण यह द्वन्द्वों के जोड़े हैं। जो मनुष्य अप्राप्त की प्राप्ति अथवा प्राप्त की सुरक्षा में संलग्न रहता है, वह मन की शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता। वह सदा अशान्त रहता है। उसके लिए आत्मकेन्द्रित होना अथवा ध्यान में लगना असम्भव है। वह सत्त्वगुण का अभ्यास नहीं कर सकता । अतः भगवान् कृष्ण अर्जुन को अर्जन-रक्षण के विचार से मुक्त हो कर शाश्वत सत्य में स्थित होने का उपदेश करते हैं। (निरूपण -IX.20, 21)
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ।।४६ ।।
शब्दार्थ : यावान् -जितना, अर्थ:-प्रयोजन, उदपाने जलाशय में, सर्वतः सर्वत्र (सब ओर), संप्लुतोदके बाद में (सब ओर जल ही जल), तावान् -उतना, सर्वेषु सब, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य-ब्राह्मण का, विजानतः ज्ञानी का ।
अनुवाद : सब ओर जल ही जल होने पर एक जलाशय का जितना महत्त्व रह जाता है, उतना ही महत्त्व अथवा प्रयोजन एक ज्ञानी ब्राह्मण का वेदों से होता है।
व्याख्या : आत्म-साक्षात्कार के उपरान्त किसी भी ऋषि-मुनि को वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता; क्योंकि उन्होंने आत्मा का अनन्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वेद निरर्थक हैं। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए नये साधकों के लिए वेदों का विशेष महत्त्व है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।४७ ।।
शब्दार्थ : कर्मणि-कर्म में, एव-ही, अधिकारः अधिकार, ते तुम्हारा, मा-नहीं, फलेषु-फल में, कदाचन-कभी, मा कर्मफलहेतुः भूः-कर्मफल तुम्हारा उद्देश्य न हो, मा-नहीं, ते तुम्हारा, सङ्गः- आसक्ति, अस्तु-हो, अकर्मणि अकर्म में।
अनुवाद : तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की इच्छा करने का कदापि नहीं। तुम्हारा उद्देश्य कर्म-फल की प्राप्ति न हो और न ही कर्म के त्याग (अकर्म) में तुम्हारा अनुराग हो।
व्याख्या : किसी भी स्थिति में कृत कर्मों के फल की आकाङ्क्षा मत करो। यदि तुम ऐसा करते हो, तो फल भोगने के लिए आवागमन के चक्र में फँसना पड़ेगा। फल की इच्छा से किया गया कर्म बन्धन में डालने वाला होता है। अनासक्त कर्म से हृदय परिमार्जित होता है। हृदय-शुद्धि से आत्म-ज्ञान प्राप्त होता है और आत्म-ज्ञान जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त कराता है।
ऐसा भी न हो कि तुम कर्म का त्याग इस भावना से करो कि जब फल ही नहीं लेना, तो कर्म कर के क्या करें।
उदार भाव में, कर्म का अभिप्राय है क्रिया । जाति अथवा जीवन में वर्ण-व्यवस्था है और आश्रम-व्यवस्था के अनुरूप कर्तव्य भी कर्म संज्ञक है। वेदों के कर्मकाण्ड के अनुयायियों (मीमांसकों) के अनुसार वेद-विहित यज्ञादि कर्म भी 'कर्म' कहलाते हैं। कर्म का रहस्य गहन है। मनुष्य की संचित वृत्तियों की नियति के आधार पर उसका भावी जन्म निर्धारित होता है।
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।।४८ ।।
शब्दार्थ : योगस्थः योग में स्थित, कुरु-करो, कर्माणि-कर्म, सङ्गम् आसक्ति, त्यक्त्वा-त्याग कर, धनञ्जय-अर्जुन, सिद्ध्यसिद्धयोः- सफलता-विफलता में, समः समभाव, भूत्वा - हो कर, समत्वम् समता, योग: योग, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : हे अर्जुन, जय-पराजय की आसक्ति त्याग कर योग में स्थित हो कर कर्म करो। मन का समत्व ही योग कहलाता है।
व्याख्या : परम देव के साथ योग में स्थित रह कर, सफलता और विफलता से ऊपर उठ कर समभाव से उसी परमात्मा के लिए कर्म करो । समत्व ही योग है। कर्मफल की इच्छा के त्याग द्वारा परिमार्जित हृदय से प्राप्त आत्म-ज्ञान ही सफलता (सिद्धि) है। कर्मफल की इच्छा से कृत कर्म द्वारा ज्ञान की प्राप्ति न होना विफलता है। (निरूपण - III.9; IV, 14, 20.)
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।।४९ ।।
शब्दार्थ : दूरेण-दूर से, हि-निश्चय से, अवरम् - निम्न श्रेणी को, कर्म-कर्म (कार्य), बुद्धियोगात् - बुद्धियोग की अपेक्षा, धनञ्जय - हे धनञ्जय, बुद्धौ-बुद्धि में, शरणम् - शरण (आश्रय), अन्विच्छ इच्छा करो, कृपणाः दयनीय, फलहेतवः-फल की आकाङ्क्षा वाले।
अनुवाद : हे अर्जुन, बुद्धियोग की अपेक्षा केवल कर्म कहीं अधिक निम्नश्रेणी का माना जाता है। तुम बुद्धि की शरण लो। फल की इच्छा रखने वाले तो कृपण हैं।
व्याख्या : समन्वित मन से किया गया कर्म बुद्धियोग है। बुद्धियोग में स्थित महात्मा जय-पराजय से प्रभावित नहीं होता। वह कर्मफल की कामना नहीं करता। वह युक्त (सम बुद्धि) हो गया है। उसकी बुद्धि आत्मस्थ हो गयी है। जहाँ किसी प्रकार के कर्म के परिणाम स्वरूप किसी भी फल की कामना नहीं होती, ऐसे बुद्धियोग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यन्त गर्हित है; क्योंकि यह जन्म-बन्धन का कारण है। (निरूपण - VIII.18)
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ।। ५० ।।
शब्दार्थ : बुद्धियुक्तः बुद्धिमान्, जहाति-त्याग देता है, इह-इस जीवन में, उभे दोनों, सुकृतदुष्कृते-अच्छे-बुरे कर्म, तस्मात्-इसलिए, योगाय-योग के लिए, युज्यस्व-संलग्न हो जाओ, योग:-योग, कर्मसु कर्मों में, कौशलम् - कुशलता, निपुणता ।
अनुवाद : बुद्धिमान् मनुष्य इसी जन्म में अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, योग-मार्ग का अनुसरण करो। योग में संलग्न हो जाओ। कर्म में कुशलता ही योग है।
व्याख्या : कर्मफल के उद्देश्य से किये गये कर्म बन्धन का कारण होते हैं; क्योंकि कर्मफल भोगने के लिए मनुष्य को पुनः जन्म लेना पड़ेगा । समभाव में किया गया कर्म अर्थात् बुद्धियोग में आत्मस्थ हो कर कृत कर्म बन्धन का कारण नहीं होता; क्योंकि परमात्मा में स्थित बुद्धि के कारण वह कर्म फल के भाव से मुक्त है और वस्तुतः वह कर्म, कर्म ही नहीं है। बन्धन में लाने वाले कर्म मन की साम्यावस्था में किये जाने पर अपनी प्रकृति त्याग देते हैं। समत्व योग में निपुण योगी सभी कर्म दिव्य अभिनेता ईश्वर को समर्पित कर देता है।
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ।।५१ ।।
शब्दार्थ : कर्मजम् -कर्म-जनित, बुद्धियुक्ताः- ज्ञानी, हि-निश्चय से, फलम् फल को, त्यक्त्वा-त्याग कर, मनीषिणः- बुद्धिमान्, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः- जन्म-बन्धन से मुक्त, पदम् -धाम, गच्छन्ति-जाते हैं, अनामयम् - दुःख रहित (सुखद) ।
अनुवाद : बुद्धिमान् मनुष्य, ज्ञान प्राप्त कर के, कर्मफल का त्याग कर देते हैं और इस प्रकार जन्म-बन्धन से विमुक्त हो कर दुःखों से परे परम धाम को प्राप्त होते हैं।
व्याख्या : कर्मफल के प्रति आसक्ति पुनर्जन्म का कारण है। कृत कर्मों का शुभाशुभ फल भोगने के लिए मनुष्य पुनः शरीर धारण करता है। यदि कोई मनुष्य कर्मफल की इच्छा त्याग कर परमात्मा के लिए अथवा उसी के ही किसी प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है, वह कर्म-बन्धन से मुक्त हो कर जन्म के बन्धन से भी मुक्त हो जाता है और शाश्वत धाम, आनन्दमयी अवस्था का अधिकारी बनता है।
मन की साम्यावस्था में रहने वाले महात्मा कर्मफल का मोह त्याग कर शुभ-अशुभ कर्मों से बच जाते हैं।
श्लोक ४९, ५०, ५१ में बुद्धि शब्द का संकेत सांख्य (ज्ञान) योग से है। इस आत्म-ज्ञान का सूर्य तब उदित होता है, जब मन कर्मयोग से परिमार्जित हो जाता है।
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।। ५२ ।।
शब्दार्थ : यदा-जब, ते-तुम्हारी, मोहकलिलम् -मोह रूपी कीचड़ को, बुद्धिः बुद्धि, व्यतितरिष्यति-तर जायेगी, तदा-तब, गन्तासि-प्राप्त करोगे, निर्वेदम् - विरक्त भाव को, श्रोतव्यस्य-सुनने योग्य के प्रति, श्रुतस्य-सुने हुए के प्रति, च-और।
अनुवाद : जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कलुषता को पार कर जायेगी, तब तुम श्रवण करने योग्य के प्रति और श्रवण किये हुए के प्रति मुक्तसङ्ग (उदासीन) हो जाओगे।
व्याख्या : आत्म-तत्त्व का अनात्मा में एकीकरण मोहकलिल है। विवेक-बुद्धि आत्मा-अनात्मा में अभेद के कारण मोह-माया में फँस जाती है और मन इन्द्रिय-विषयों की ओर भागता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य शरीर को ही आत्मा समझने की भूल कर बैठता है। मन पवित्र होने पर मनुष्य श्रुत और अश्रुत के प्रति उदासीन हो जाता है। इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उन सबके प्रति अर्थात् शास्त्रों के प्रति उसमें उदासीनता आ जाती है। (निरूपण-XVI.24)
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।।५३ ।।
शब्दार्थ : श्रुतिविप्रतिपन्ना-सुने हुए के प्रति किंकर्तव्यविमूढ़, ते तुम्हारी, यदा-जब, स्थास्यति-स्थिर हो जायेगी, निश्चला-एकनिष्ठ, समाधौ-आत्मा में, अचला-स्थिर, बुद्धिः बुद्धि, तदा-तब, योगम्-योग को, अवाप्स्यसि-प्राप्त करोगे।
अनुवाद : वेद-शास्त्रों के श्रवण से किंकर्तव्यविमूढ़ हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर और आत्मस्थ हो जायेगी, तभी तुम्हें अन्तर्ज्ञान व आत्म-साक्षात्कार होगा।
व्याख्या : प्रवृत्ति-मार्ग और निवृत्ति-मार्ग में विचारों के विरोधाभास के कारण जो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गयी है, उसके विक्षेप और शंका समाप्त होने पर तथा बुद्धि के आत्मा में स्थिर होने पर तुम्हें आत्म-ज्ञान होगा।
अर्जुन उवाच
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ।।५४ ।।
शब्दार्थ : स्थितप्रज्ञस्य-अचल बुद्धि वाले (महात्मा की), का-क्या, भाषा-भाषा (लक्षण), समाधिस्थस्य-परा चेतना में लीन पुरुष की, केशव-हे कृष्ण, स्थितधीः - स्थिर बुद्धि वाले, किम् -कैसे, प्रभाषेत-बोलता है, किम् -कैसे, आसीत-बैठता है, व्रजेत-चलता है, किम् -कैसे।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले समाधि (परा चेतना) में स्थित महात्मा के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे विचरण करता है?
व्याख्या : अर्जुन भगवान् कृष्ण से यह जानने का इच्छुक है कि स्थिरधीः पुरुष जो आत्मस्थ है, उसके लक्षण क्या हैं। वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है।
अचल मति पुरुष के लक्षण और आत्मा के उस स्थिर ज्ञान को प्राप्त करने के उपाय इस अध्याय के श्लोक ५५ से ७२ तक वर्णित हैं।
स्थिर बुद्धि का ज्ञान भगवत्साक्षात्कार अथवा ब्रहौक्य द्वारा प्रतिष्ठित ज्ञान है। (निरूपण-XIV.21, 27)
श्री भगवानुवाच
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। ५५ ।।
शब्दार्थ : प्रजहाति-त्याग देता है, यदा-जब, कामान् इच्छाओं को, सर्वान् सभी, पार्थ- हे पार्थ, मनोगतान् - मन की, आत्मनि-आत्मा में, एव-ही, आत्मना आत्मा से, तुष्टः सन्तुष्ट, स्थितप्रज्ञः - स्थिर बुद्धि वाला, तदा-तब, उच्यते-कहा जाता है।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : हे पार्थ, जब मनुष्य मन की सर्व कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही सन्तुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ अर्थात् स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है।
व्याख्या : इस श्लोक में भगवान् कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर देते हैं।
यदि किसी व्यक्ति को मिश्री मिल जाये, तो क्या वह गुड़ की चाह करेगा ? कदापि नहीं। यदि कोई आत्मा का आनन्द प्राप्त कर सकता है, तो क्या वह ऐन्द्रिक सुखों की लालसा करेगा? नहीं, कदापि नहीं। आत्मा में ही सन्तुष्ट महात्मा को, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, संसार के समस्त ऐश्वर्य भी व्यर्थ लगेंगे।
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।।५६ ।।
शब्दार्थ : दुःखेषु दुःखों में, अनुद्विममनाः-अविचलित मन वाला, सुखेषु सुखों में, विगतस्पृहः- लालसा रहित, वीतरागभयक्रोधः राग, भय, क्रोध से मुक्त, स्थितधी:- स्थिर बुद्धि वाला, मुनिः - मुनि, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : जिसका मन कष्टों से विचलित नहीं होता, जो ऐन्द्रिक सुखों की लालसा से मुक्त है, जो आसक्ति, भय और क्रोध से भी मुक्त है, वह मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है।
व्याख्या : भगवान् कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले मुनि के लक्षण बताते हुए अर्जुन के प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देते हैं।
स्थितधी मुनि का मन विपत्ति काल में अधीर नहीं होता। वह आध्यात्मिक ताप (शरीर में होने वाले रोगों से), अधिदैविक ताप (मेघगर्जन, विद्युत, तूफान, बाढ़ आदि) और अधिभौतिक ताप (शेर, चीता, सर्प, बिच्छू आदि) से अर्थात् तीनों तापों से प्रभावित नहीं होता । समृद्ध अवस्था में वह इन्द्रिय-सुख की कामना नहीं करता। (निरूपण-IV.10)
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।५७ ।।
शब्दार्थ : यः जो, सर्वत्र-सभी स्थान, अनभिस्नेहः अनासक्त, तत्-तत्-वह-वह, प्राप्य-प्राप्त कर के, शुभाशुभम् - शुभ और अशुभ, न नहीं, अभिनन्दति-प्रसन्न होता है, न-नहीं, द्वेष्टि-द्वेष करता है, तस्य-उसकी , प्रज्ञा-बुद्धि, प्रतिष्ठिता- स्थिर है।
अनुवाद : जो सर्वत्र, सब स्थान पर आसक्ति रहित है, शुभ अथवा अशुभ फल मिलने पर जो न तो प्रसन्न होता है और न ही दुःखी होता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है (स्थिर है) ।
व्याख्या : मुनि के पास मन का समत्व होता है। न तो सुख आने पर वह प्रसन्न होता है और न ही दुःख आने पर विचलित होता है। आत्मा में प्रतिष्ठित होने के कारण वह (संसार से) उदासीन रहता है। उसे अपने शरीर अथवा जीवन से भी अनुराग नहीं होता, क्योंकि वह तो ब्रह्म में स्थित रहता है। कोई उसके लिए अच्छा करे, तो वह उसकी प्रशंसा नहीं करता और बुरा करने वाले से वह द्वेष भी नहीं करता। "स्थितधी मुनि कैसे बोलता है", अर्जुन के प्रश्न का भगवान् ने इस प्रकार उत्तर दिया।
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।५८ ।।
शब्दार्थ : यदा-जब, संहरते-संहरण कर लेता है (समेट लेता है), च-और, अयम्यह, कूर्म:-कछुआ, अङ्गानि अङ्गों को, इव-समान, सर्वशः सब ओर से, इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ, इन्द्रियार्थेभ्यः - विषयों से, तस्य-उसकी, प्रज्ञा-बुद्धि, प्रतिष्ठिता-स्थिर ।
अनुवाद : चारों ओर से अपने अङ्गों का संहरण कर लेने वाले कछुए की भाँति जब कोई पुरुष इन्द्रियों के विषयों से अपनी इन्द्रियों को विमुख कर लेता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला, प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला कहलाता है।
व्याख्या : इन्द्रियों का संहरण प्रत्याहार है। बाह्य विषयों की ओर भागना मन की स्वाभाविक वृत्ति है। योगी पुनः पुनः मन को उसके विषयों से हटा कर आत्मा में स्थिर करता है। प्रत्याहार की शक्ति से युक्त योगी किसी सामूहिक स्थान पर भी इन्द्रियों को अन्तर्मुख कर के पलक झपकते ही समाधि में प्रवेश कर सकता है। वह किसी भी प्रकार के कोलाहल अथवा ध्वनियों से विचलित नहीं होता। युद्धक्षेत्र में भी प्रत्याहार द्वारा वह अपने केन्द्र, आत्मा में विश्राम ले सकता है। प्रत्याहार का अभ्यासी संसार के लिए मृत है। बाह्य ऊर्मियों (तरङ्गों) से वह प्रभावित नहीं होगा। आत्म-शक्ति से वह किसी भी समय अपनी इन्द्रियों को पूर्ण रूप से वशीभूत करने में समर्थ है। वे तो मानो उसकी आज्ञाकारी सेविकाएँ हैं अथवा साधन मात्र हैं।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ।।५९ ।।
शब्दार्थ : विषयाः - इन्द्रियों के विषय, विनिवर्तन्ते-विमुख हो जाते हैं, निराहारस्य-जितेन्द्रिय के, देहिनः-उस पुरुष के, रसवर्जम् - आसक्ति को पीछे छोड़ते हुए (रस का त्याग), रस:-रस (आनन्द), अपि-भी, अस्य-उसके, परम् - उत्कृष्ट, दृष्ट्वा-देख कर, निवर्तते-समाप्त हो जाता है।
अनुवाद : जितेन्द्रिय पुरुष के विषय तो निवृत हो जाते हैं; किन्तु उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है। स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी ब्रह्मसाक्षात्कार कर के निवृत्त हो जाती है।
व्याख्या : आत्म-ज्ञान ही सूक्ष्म वासनाओं (सुप्त वृत्तियों) को पूर्ण रूप से नष्ट कर सकता है। सूक्ष्म कामनाओं, आसक्तियों और विषयों की लालसा भी आत्म-ज्ञान होने पर शून्य हो जाती है। कठोर तप द्वारा इन्द्रियों के विषय परावर्ती हो जाते हैं; परन्तु महात्मा के हृदय में सुप्त रूप से उनका स्वाद, उनकी आकाङ्क्षा पुनरपि रह ही जाती है।
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ।।६० ।।
शब्दार्थ : यततः यत्न करते हुए, हि-निश्चित रूप से, अपि-भी, कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र, पुरुषस्य मनुष्य की, विपश्चितः बुद्धिमान् की, इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ, प्रमाथीनि-प्रबल, हरन्ति-हर लेती हैं, प्रसभम् बलपूर्वक, मनः मन ।
अनुवाद : हे अर्जुन, सतत यत्न करते रहने पर भी ये चंचल इन्द्रियाँ बुद्धिमान् पुरुष के मन को हठात् हर लेती हैं।
व्याख्या : साधक को चाहिए कि प्रथम तो वह अपनी इन्द्रियों को संयत करे । इन्द्रियों को घोड़े की संज्ञा दी जाती है। घोड़े को अपने पूर्ण वश में करने की सामर्थ्य होने पर ही तुम अपने गन्तव्य तक पहुँच सकते हो। असंयत घोड़े तो तुम्हें मार्ग में ही नीचे गिरा देंगे। इसी प्रकार से चंचल इन्द्रियाँ तुम्हें इन्द्रिय-विषयों के भँवर में फँसा कर तुम्हारे आध्यात्मिक लक्ष्य-मोक्ष और शाश्वत शान्ति के परम धाम से पतन करा देंगी। (निरूपण -III.33; V.14)
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।६१ ।।
शब्दार्थ : तानि-उन, सर्वाणि-सब को, संयम्य-वशीभूत कर के, युक्तः लगा कर, आसीत -बैठना चाहिए, मत्परः- मुझ में ध्यान लगा कर, वशे-वश में, हि-निश्चयेन, यस्य-जिसकी, इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ, तस्य-उसकी, प्रज्ञा-बुद्धि, प्रतिष्ठिता- स्थिर है।
अनुवाद : इन्द्रियों को वश में कर के मुझ में ध्यान लगा कर स्थिरतापूर्वक बैठना चाहिए; क्योंकि बुद्धि उसी की स्थिर होती है जिसकी इन्द्रियाँ संयत हैं।
व्याख्या : जितेन्द्रिय बन कर शान्त मन से मुझ में चित्त एकाग्र कर के आसन में बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रतिष्ठित योगी जिसने अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया है, निस्सन्देह अत्यन्त स्थिर है। वह आत्मा में स्थित है। श्री शंकराचार्य ने 'आसीत मत्परः' की व्याख्या इस प्रकार की है- "उसे यह ध्यान करते हुए बैठना चाहिए कि 'मैं उस (परमात्मा) से पृथक् नहीं हूँ।" (निरूपण -11.64)
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ।।६२ ।।
शब्दार्थ : ध्यायतः-चिन्तन करते हुए, विषयान् - विषयों का, पुंसः मनुष्य का, सङ्गः- आसक्ति, तेषु उनमें, उपजायते-उत्पन्न होती है, सङ्गात् आसक्ति से, सञ्जायते-जन्म लेती है, काम:-इच्छा, कामात् इच्छा से, क्रोधः क्रोध, अभिजायते - प्रकट होता है।
अनुवाद : विषयों का चिन्तन करने पर उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा विकसित होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है।
व्याख्या : जब कोई मनुष्य किसी सुन्दर, सुखद, मनोहारी वस्तु का चिन्तन करता है, तो उसके प्रति उसके मन में आसक्ति उत्पन्न होती है और उसे प्राप्त करने योग्य समझ कर वह उसे पाने की स्पृहा (अभिलाषा) करता है। उस पर अधिकार पाने का पूर्ण प्रयास कर के वह उसकी प्राप्ति हेतु संघर्ष करता है। किसी कारणवश इच्छा पूर्ण न होने पर वह क्रोधित हो उठता है। वस्तु-प्राप्ति में कोई उसकी राह में बाधा डाले, तो वह उत्तेजित हो उठता है, उससे द्वन्द्व करता है और उसका वैरी हो जाता है। (निरूपण - 11.64)
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।।६३ ।।
शब्दार्थ : क्रोधात् -क्रोध से, भवति-होता है, सम्मोहः मोह, सम्मोहात् -मोह से, स्मृतिविभ्रमः स्मृतिनाश, स्मृतिभ्रंशात् स्मृतिनाश से, बुद्धिनाशः-विवेक का नाश, बुद्धिनाशात् - विवेक नष्ट होने पर, प्रणश्यति नष्ट हो जाता है।
अनुवाद : क्रोध से मूढ़भाव (मोह) उत्पन्न होता है, मोह से स्मृतिलोप होता है, स्मृतिलोप से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से मनुष्य का ही विनाश हो जाता है।
व्याख्या : क्रोध मोह का कारण है। क्रोध आने पर व्यक्ति सदसद विवेक खो बैठता है। वह अपनी इच्छा के अनुरूप बोलेगा और कार्य करेगा। भावुकता और आसक्ति उसके विनाश का कारण बन जायेंगी और वह अज्ञानी जैसा व्यवहार करेगा।
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।।६४ ।।
शब्दार्थ : रागद्वेषवियुक्तैः राग (आसक्ति) और द्वेष से मुक्त, तु-किन्तु, विषयान् विषयों को, इन्द्रियैः इन्द्रियों के द्वारा, चरन् -विचरण करता हुआ (भोगता हुआ), आत्मवश्यैः संयत, विधेयात्मा संयमी पुरुष, प्रसादम् -शान्ति, अधिगच्छति-प्राप्त करता है।
अनुवाद : किन्तु संयमी पुरुष अपनी इन्द्रियों को वश में कर के, आसक्ति और विरक्ति से मुक्त रह कर विषयों में विचरण करता हुआ भी अर्थात् विषयों को भोगता हुआ भी परमात्मा के प्रसाद को प्राप्त करता है।
व्याख्या : मन और इन्द्रियाँ प्रकृतिवश ही आसक्ति और विरक्ति की दो धाराओं से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि मन और इन्द्रियों को कुछ विषयों से तो लगाव है और अन्य कतिपय विषयों के प्रति विरक्त भाव है। किन्तु एक अनुशासित मनुष्य अपने मन और इन्द्रियों को वशीभूत कर के ही विषयों में विचरता है। राग-द्वेष से ऊपर उठ कर आत्मा के प्रभुत्व में वह शाश्वत शान्ति प्राप्त करता है। अनुशासित आत्मा की इच्छा-शक्ति प्रबल होने के कारण मन और इन्द्रियाँ उसके आधिपत्य में रहती हैं। अनुशासित आत्मा, प्रेम और घृणा को त्याग कर केवल उन्हीं विषयों का भोग करता है जो शरीर को चलाने के लिए अनिवार्य है। वह शास्त्र द्वारा निषिद्ध विषयों का उपभोग नहीं करता।
इस श्लोक में भगवान् कृष्ण अर्जुन के चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देते हैं-"स्थितप्रज्ञ कैसे विचरण करता है?" (निरूपण-III.7, 19, 25; XVIII.9)
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।।६५ ।।
शब्दार्थ : प्रसादे-शान्ति में, सर्वदुःखानाम् -सब दुःखों का, हानिः-विनाश, अस्य-उसके, उपजायते-हो जाता है, प्रसन्नचेतसः-प्रसन्न मन वाले, हि-क्योंकि, आशु-शीघ्र, बुद्धिः - बुद्धि, पर्यवतिष्ठते-स्थिर हो जाती है।
अनुवाद : उस शान्ति में सब दुःख नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि प्रशान्त मन वाले की बुद्धि शीघ्र ही आत्मस्थ (आत्मा में स्थिर) हो जाती है।
व्याख्या : मन की शान्ति होने पर विषयों के पीछे भाग-दौड़ समाप्त हो जाती है। योगी को अपनी विवेक-बुद्धि पर पूर्ण अधिकार (प्रभुत्व) होता है। बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाती है। यह अत्यन्त स्थिर हो जाती है। शरीर और मन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ।। ६६ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, अस्ति-है, बुद्धिः बुद्धि, अयुक्तस्य-अस्थिर पुरुष की, ननहीं, च-और, अयुक्तस्य-अस्थिर की, भावना-ध्यान, ननहीं, च-और, अभावयतः- भावना रहित (मनुष्य को), शान्तिः शान्ति, अशान्तस्य-जिसे शान्ति न हो, कुतः-कहाँ से, सुखम् -सुख ।
अनुवाद : अयुक्त मनुष्य में बुद्धि और भावना का अभाव होता है। भाव के अभाव में न तो ध्यान एकाग्र हो सकता है और न ही शान्ति मिल सकती है। शान्ति के अभाव में सुख की कामना कैसे कर सकते हैं?
व्याख्या : ध्यानस्थ हुए बिना व्यक्ति आत्म-ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । अनिश्चयात्मिका बुद्धि से युक्त मनुष्य ध्यानाभ्यास नहीं कर सकता। न तो उसमें आत्म-ज्ञान की तड़प होती है और न ही मोक्ष के लिए उत्कट आकाङ्क्षा । ध्यान न करने वाला व्यक्ति शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता और अशान्त व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता।
इच्छा और तृष्णा (ऐन्द्रिक विषयों की पिपासा) शान्ति की शत्रु है। भौतिक सुखों की लालसा करने वाला किंचिन्मात्र भी सुख की अभिलाषा नहीं कर सकता । मन तो सदा अशान्त है, विषयों की ओर दौड़ रहा है। केवल इस तृष्णा के शान्त होने पर ही वास्तविक शान्ति का सुख प्राप्त किया जा सकता है। तभी मन एकाग्र होगा, ध्यान में आनन्द आयेगा और आत्मा में स्थिति होगी।
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ।।६७ ।।
शब्दार्थ : इन्द्रियाणाम् - इन्द्रियों में, हि-निश्चय से, चरताम् - विचरण करते हुए, यत्-जो, मनः-मन, अनुविधीयते-अनुसरण करता है, तत् - उसे, अस्य-उसकी, हरति-हर लेती है, प्रज्ञाम् - विवेक-शक्ति को, वायुः- वायु, नावम् नाव को, इव-समान, अम्भसि-जल में।
अनुवाद : इतस्ततः भटकती इन्द्रियों का अनुगामी मन (मनुष्य की) बुद्धि का उसी प्रकार हरण कर लेता है जैसे जल में पड़ी नौका को वायु (बहा) ले जाता है।
व्याख्या : इन्द्रियों के सङ्ग रमण करने वाला और सतत विषय-वासनाओं का चिन्तन करने वाला मन मनुष्य के विवेक को पूर्णतया नष्ट कर देता है। जिस प्रकार वायु नाव को अपने मार्ग से दूर ले जाता है, उसी प्रकार मन साधक को आध्यात्मिक पथ से विचलित कर के भौतिक विषयों की ओर उन्मुख कर देता है।
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ६८ ।।
शब्दार्थ : तस्मात् - इसलिए, यस्य-जिसकी, महाबाहो -पराक्रमी अर्जुन, निगृहीतानि-संयत कर ली गयी हों, सर्वशः- पूर्णतया, इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ, इन्द्रियार्थेभ्यः- इन्द्रिय-विषयों से, तस्य-उसकी, प्रज्ञा-ज्ञान, प्रतिष्ठिता-स्थिर ।
अनुवाद : अतः हे अर्जुन, ज्ञान उसका ही स्थिर है जिसकी इन्द्रियाँ विषयों से पराङ्मुख और संयत हैं।
व्याख्या : इन्द्रियाँ पूर्ण रूप से संयत हों, तो मन वासनाओं के घने जंगल में उन्मत्त हो कर विचरण नहीं करता । वात रहित स्थान पर दीपक की भाँति यह स्थिर हो जाता है। तब योगी आत्मस्थ हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। (निरूपण-III.7)
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।।६९ ।।
शब्दार्थ : या जो, निशा-रात्रि, सर्वभूतानाम् -सब प्राणियों की, तस्याम् उसमें, जागर्ति-जागता है, संयमी-संयत पुरुष, यस्याम् - जिसमें, जाग्रति-जागते हैं, भूतानि-प्राणी, सा-वह, निशा-रात्रि, पश्यतः क्रान्तदर्शी (तत्त्वदर्शी) के लिए, मुनेः मुनि के लिए।
अनुवाद : समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें जितेन्द्रिय पुरुष जागता है। जिसमें और प्राणी जागते हैं, वह आत्म-निरीक्षण करने वाले मुनि के लिए रात्रि है।
व्याख्या : सांसारिक प्रपंच में उलझे हुए व्यक्ति के लिए जो वास्तविकता है, वह मुनि के लिए भ्रम है और जो मुनि के लिए वास्तविकता है, वह संसारी के लिए भ्रम है। मुनि आत्म-निष्ठ होता है। यही उसका दिन है अर्थात् आत्मा में स्थिति। वह भौतिक परिवेश से अनभिज्ञ रहता है। वह उसके लिए रात्रि है। सामान्य व्यक्ति अपनी सत्य प्रकृति से अनभिज्ञ है। आत्मा में स्थिति उसकी रात्रि है। वह तो ऐन्द्रिक विषयों का सुख-भोग करता रहता है। यही उसका दिन है। उसके लिए आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। मुनि के लिए विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है।
आत्म-ज्ञान से शून्य होने के कारण भौतिक जगत् के लोग घोर अन्धकार में पड़े हैं। उनके लिए जो अन्धकार है, जितेन्द्रिय के लिए वह प्रकाश है। आत्मा और ब्रह्म संसार के लिए रात्रि के समान हैं; किन्तु ज्ञानी तो उसमें पूर्णतः जागृत है। वह प्रकाशों के प्रकाश का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रहा है। वह ज्योतिर्मय हो गया है। आत्मज्ञानी हो गया है।
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।।७० ।।
शब्दार्थ : आपूर्यमाणम् -सर्वतः परिपूर्ण, अचलप्रतिष्ठम् -मर्यादित, स्थिर, समुद्रम् -सागर, आपः- जल, प्रविशन्ति-प्रवेश करते हैं, यद्वत्-जैसे, तद्वत्-वैसे, कामाः इच्छाएँ, यम् - जिसमें, प्रविशन्ति-प्रवेश करती है सर्वे-सब, सः वह, शान्तिम् - शान्ति को, आप्नोति - प्राप्त करता है,न-नहीं, कामकामी-कामनाओं का इच्छुक ।
अनुवाद : जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण अचल, स्थिर सागर में जला (उसे क्षुब्ध किये बिना) प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य में सब कामनाएँ उसे विचलित किये बिना प्रवेश कर जाती हैं, वह शान्ति को प्राप्त करता है, कामनाओं का इच्छुक नहीं।
व्याख्या : सब ओर से जल से परिपूर्ण समुद्र जिस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, स्थिर, शान्त बना रहता है, उसी प्रकार स्व-स्वरूप में स्थित पुरुष उसमें सब ओर से प्रवेश करने वाली कामनाओं से प्रभावित नहीं होता। ऐसा स्थितप्रज्ञ पुरुष ही शान्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। विषयों के भोग में आनन्द लेने वाला अथवा कामेच्छुक व्यक्ति कदापि शान्ति प्राप्त करने का स्वप्न नहीं देख सकता। (निरूपण-XVIII. 53, 54)
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।।७१ ।।
शब्दार्थ : विहाय-त्याग कर, कामान्-इच्छाओं को, यः जो, सर्वान् -सब, पुमान् मनुष्य, चरति- विचरण करता है, निःस्पृहः-कामना रहित, निर्ममः अहंभाव से शून्य, निरहंकारः- अभिमान रहित, सः- वह, शान्तिम् - शान्ति (को), अधिगच्छति-प्राप्त करता है ।
अनुवाद : समस्त इच्छाओं का परित्याग कर के, लालसा रहित, ममत्व भाव से रहित व अहंकारशून्य मनुष्य ही शान्ति प्राप्त कर सकता है।
व्याख्या : आप्तकाम पुरुष जिसने सब इच्छाएँ त्याग दी हैं, जो 'मैं' और 'मेरा' भाव से ऊपर उठ गया है, जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में ही सन्तुष्ट है और उनकी भी चिन्ता नहीं करता अथवा उन आवश्यकताओं के प्रति भी पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाता है, वह शाश्वत शान्ति अथवा मोक्ष का अधिकारी होता है। (निरूपण—II.55)
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।।७२ ।।
शब्दार्थ : एषा-यह, ब्राह्मी-ब्राह्निक (आध्यात्मिक), स्थितिः- अवस्था, पार्थ-हे पार्थ, न नहीं, एनाम्-इसे, प्राप्य-प्राप्त कर के, विमुह्यति-मोहित होता है, स्थित्वा-स्थित हो कर, अस्याम् - इसमें, अन्तकाले-मृत्यु के समय, अपि-भी, ब्रह्मनिर्वाणम् -ब्रह्म के साथ एकत्व, ऋच्छति -प्राप्त करता है।
अनुवाद : हे पार्थ (अर्जुन), यही ब्राह्मी स्थिति (शाश्वत दिव्य अवस्था) है। इसे प्राप्त करने पर कोई मोह में नहीं फँसता । इसमें प्रतिष्ठित हो कर मनुष्य अन्त काल (मृत्यु के समय) में ब्रह्मैक्य (निर्वाण) प्राप्त करता है।
व्याख्या : पूर्व श्लोक में वर्णित अवस्था-सर्वस्व त्याग और ब्रह्म में स्थिति ही ब्राह्मी स्थिति है। इस अवस्था को प्राप्त करने के उपरान्त व्यक्ति मोहित नहीं होता । मृत्यु के समय भी यदि वह इसी अवस्था में रहता है, तो मोक्ष प्राप्त करता है। यह कहना अनिवार्य नहीं कि जीवन-भर ब्रह्मभाव में स्थित रहने वाला व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति अथवा ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्ति करता है। (निरूपण-VIII.5, 6)
विद्यारण्य मुनि पंचदशी में कहते हैं कि यहाँ 'अन्तकाल' का अभिप्राय उस क्षण से है जो अविद्यानाश अथवा देह और देही के परस्पर न्यास की समाप्ति का है।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।।
।। इति सांख्ययोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ तृतीयोऽध्यायः
कर्मयोगः
अर्जुन उवाच
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।।१ ।।
शब्दार्थ : ज्यायसी-श्रेष्ठतर, चेत्-यदि, कर्मणः-कर्म से, ते-आपके द्वारा, मता-समझी जाती है, बुद्धिः बुद्धि, जनार्दन-हें जनार्दन, तत्-फिर, किम् -क्यों, कर्मणि-कर्म में, घोरे-भयंकर, माम्-मुझे, नियोजयसि लगाते हो, केशव-हे केशव ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे कृष्ण, यदि आप सोचते हैं कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठतर है तो हे केशव, मुझे इस भयानक कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं?
व्याख्या : अध्याय २ के श्लोक ४९, ५० और ५१ में भगवान् कृष्ण ने ज्ञानयोग के सन्दर्भ में उत्कृष्ट वचन कहे हैं। वे पुनः अर्जुन को युद्ध के लिए कह रहे हैं। इसी कारण से अर्जुन भ्रमित हो रहा है।
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ।।२ ।।
शब्दार्थ : व्यामिश्रेण-सम्भ्रमित करने वाली, इव-मानो, वाक्येन-वाणी के द्वारा, बुद्धिम् बुद्धि को, मोहयसि-मोहित कर रहे हो, इव-मानो, मे—मेरी, तत्-वह, एकम् - एक, वद-बोलो, निश्चित्य-निश्चय करके, येन-जिससे, श्रेयः आनन्द (कल्याण), अहम् -मैं, आप्नुयाम् - प्राप्त करूँ ।
अनुवाद : भ्रमित करने वाली आपकी इस प्रकट वाणी से मानो आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से उस एक वचन को मेरे लिए कहें जो मेरे लिए कल्याणप्रद हो, जिससे मैं आनन्दमग्न हो सकूँ।
व्याख्या : अर्जुन भगवान् कृष्ण से कहते हैं- "ज्ञान अथवा कर्म, इन दोनों में से मुझे एक का उपदेश दीजिए, जिससे मैं सर्वोच्च कल्याण, आनन्द अथवा मोक्ष का अधिकारी बन सकूँ।" (निरूपण-V.1)
श्री भगवानुवाच
लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ।।३ ।।
शब्दार्थ : लोके-लोक में, अस्मिन् - इस (में), द्विविधा-दो प्रकार की, निष्ठा-आस्था, पुरा-पूर्वकाल में, प्रोक्ता-कही गयी, मया-मेरे द्वारा, अनघ हे निष्पाप, ज्ञानयोगेन -ज्ञानयोग के द्वारा, सांख्यानाम् - ज्ञानियों की, कर्मयोगेन कर्मयोग के द्वारा, योगिनाम् - योगियों की।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : हे अनघ (निष्पाप), इस लोक में, पूर्वकाल में मैंने दो प्रकार की निष्ठा का उपदेश दिया था। उनमें सांख्य जनों (ज्ञानी अथवा चिन्तनशील) की निष्ठा तो ज्ञान-मार्ग में है और योगियों की निष्ठा कर्म-मार्ग में है।
व्याख्या : सांख्यों का ज्ञानयोग भगवान् कृष्ण के द्वारा अध्याय २ के श्लोक ११ से ३८ और कर्मयोग ४० से ५३ में वर्णित है।
पुरा प्रोक्ता का यह अभिप्राय भी हो सकता है कि 'सृष्टि के आदिकाल में मैंने इन दोनों प्रकार के योगों का ज्ञान संसार को दिया था।
साधन चतुष्टय और तीव्र सूक्ष्म बुद्धि तथा साहसिक मेधा से युक्त व्यक्ति ही ज्ञान-मार्ग (योग) का अनुसरण कर सकते हैं। कर्मशील व्यक्ति कर्मयोग के लिए उपयुक्त है।
साधन चतुष्टय हैं-विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत् और मुमुक्षुत्व । षट् सम्पत् हैं-शम (मनोनिग्रह), दम (इन्द्रियनिग्रह), तितिक्षा (सहनशीलता), उपरति (विषयों से विमुखता), श्रद्धा और समाधान ।
एक काल में दो योगों का अभ्यास सम्भव नहीं है। कर्मयोग किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। यह हृदय को पवित्र करके साधक को ज्ञान-प्राप्ति के योग्य बनाता है। हृदय पवित्र होते ही कर्मयोगी को ज्ञानयोग अपना लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की बाह्य सहायता के बिना ज्ञानयोग साधक को सीधा उसके लक्ष्य तक पहुँचाता है। (निरूपण - V.5)
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते ।
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ।।४।।
शब्दार्थ : न-नहीं, कर्मणाम् -कर्मों के, अनारम्भात् - प्रारम्भ न करने से, नैष्कर्म्यम् -कर्म से मुक्ति, पुरुषः- मनुष्य, अश्नुते-प्राप्त करता है, न-नहीं, च-और, संन्यसनात् - त्याग से, एव-ही, सिद्धिम् -सिद्धि (पूर्णता), समधिगच्छति -प्राप्त करता है।
अनुवाद : कोई भी मनुष्य कर्म के न करने से नैष्कर्म्यता (जिसमें मनुष्य पर कर्म का कोई प्रभाव ही न पड़े, ऐसी अवस्था) को प्राप्त नहीं हो सकता और न ही कर्म से संन्यास ले कर अर्थात् कर्म का त्याग कर के वह पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है।
व्याख्या : नैष्कर्म्यम् और सिद्धि पर्यायवाची शब्द हैं। नैष्कर्म्यता अथवा पूर्णत्व को प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष अपनी वास्तविक प्रकृति सच्चिदानन्द (सत्-चित्-आनन्द) स्वरूप में स्थित होता है। किसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म की न तो उसकी कोई कामना होती है और न आवश्यकता। वह आप्तकाम होता है।
आत्म-ज्ञान के द्वारा मनुष्य निष्कर्मण्यता की अवस्था को प्राप्त करता है। कर्मत्याग कर के कोई मनुष्य केवल शान्त हो कर बैठ जाये, तो ऐसा नहीं है कि उसने इस उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लिया है। प्रपंचानुराग में फँसा उसका मन तो कई प्रकार की योजनाएँ बना रहा होगा। विचार ही वास्तव में कर्म है। सकारात्मक विचार, तृष्णा, इच्छा-अनिच्छा से मुक्त ज्ञानी पुरुष ही नैष्कर्म्यता की अवस्था को पा सकता है।
आत्म-ज्ञान के बिना मात्र कर्म के त्याग द्वारा पूर्णता अथवा मोक्ष-प्राप्ति असम्भव है। (निरूपण - XVIII.49)
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।।५।।
शब्दार्थ : न हि-नहीं, कश्चित् -कोई, क्षणम् -क्षण, अपि-भी, जातु-निश्चित रूप से, तिष्ठति-रहता है, अकर्मकृत्-बिना कर्म किये, कार्यते-किया जाता है, हि-क्योंकि, अवशः - विवश हो कर, कर्म-कर्म, सर्वः-सब, प्रकृतिजैः - प्रकृति से उत्पन्न, गुणैः- गुणों के द्वारा।
अनुवाद : निश्चित रूप से कोई भी मनुष्य बिना कर्म किये एक क्षण भी नहीं रह सकता; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण विवश हो कर कर्म करना ही पड़ता है।
व्याख्या : सत्त्व, रजस् और तमस् प्रकृति के तीन गुण हैं। सत्त्व- समन्वय, शुचिता अथवा प्रकाश का प्रतीक है। रजस्-आसक्ति अथवा क्रियाशीलता का प्रतीक है। तमस् - अन्धकार अथवा जड़ता है। सात्त्विक कर्म मोक्ष-प्राप्ति में सहायक होते हैं। राजसिक और तामसिक कर्म मनुष्य को संसार के बन्धन में डालते हैं।
आत्म-ज्ञानी को ये गुण प्रभावित नहीं करते। वह इन गुणों से परे हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। अज्ञानान्धकार में पड़ा व्यक्ति जिसके पास स्व-आत्मा का प्रकाश नहीं है अथवा जो आत्म-ज्ञान से शून्य है और अविद्या द्वारा अनुशासित है, असहाय रूप से गुणों में विचरण करने को बाध्य होता है। (निरूपण - IV.16; XVIII.11)
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।।६ ।।
शब्दार्थ : कर्मेन्द्रियाणि-कर्मेन्द्रियों को, संयम्य-वशीभूत करके, यः-जो, आस्ते-रहता है, मनसा-मन से, स्मरन्-स्मरण करता हुआ, इन्द्रियार्थान् - इन्द्रियों के विषयों को, विमूढात्मा-भ्रमित बुद्धि वाला, मिथ्याचार:- दम्भी, सः- वह, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : जो मनुष्य (पाँच) कर्मेन्द्रियों को तो नियन्त्रित कर लेता है; परन्तु मन से कर्मेन्द्रियों के विषयों में रमण करता रहता है, उनका चिन्तन करता है. ऐसा मनुष्य मिथ्या आचरण वाला कहलाता है, क्योंकि वह भ्रम में पड़ा हुआ है।
व्याख्या : पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं-वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ और गुदा। ये सूक्ष्म तत्त्वों अथवा राजसिक गुण के पाँच तन्मात्राओं से अंकुरित होती हैं। वाक् (शब्द) आकाश तन्मात्रा से, पाणि-वायु तन्मात्रा से, पाद-अधि तन्मात्रा से, उपस्थ-आपस् (जल) तन्मात्रा से और गुदा-पृथ्वी तन्मात्रा से उद्भुत है। वह मनुष्य पापाचारी है जो शान्त बैठ कर मन से इन्द्रिय-विषयों का चिन्तन करता रहता है। वह स्वयं में भ्रमित है। निश्चित रूप से सम्मोहित है।
कर्मेन्द्रियों को संयत कर के विचारों को नियन्त्रित करना भी अनिवार्य है। मन को भगवान् में लगाना चाहिए। एकाग्रता से ही मनुष्य सच्चा योगी बन सकता है और तभी आत्मानुभूति सम्भव है।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।।७ ।।
शब्दार्थ : यः -जो, तु-किन्तु, इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को, मनसा-मन से, नियम्य-संयत कर के, आरभते-प्रारम्भ करता है, अर्जुन-हे अर्जुन, कर्मेन्द्रियैः- कर्मेन्द्रियों से, कर्मयोगम् -कर्मयोग को, असक्तः - अनासक्त, सः- वह, विशिष्यते-उत्कृष्ट है।
अनुवाद : इन्द्रियों को संयत कर के जो मनुष्य अनासक्त हो कर कर्मेन्द्रियों को कर्म में लगा कर स्वयं कर्मयोग में प्रतिष्ठित होता है, वह श्रेष्ठ है।
व्याख्या : हस्त, पाद, वाक् आदि कर्मेन्द्रियों से कर्म करते हुए ज्ञानेन्द्रियों को मन से वशीभूत कर के, कर्मफल त्याग कर और अहंकारशून्य हो कर जो मनुष्य कर्म करता है, वह निस्सन्देह मिथ्याचारी (दम्भी) से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। (निरूपण-II. 64, 68; IV.21.)
नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा और रसना पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं।
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ।।८ ।।
शब्दार्थ : नियतम् - शास्त्रविहित, कुरु-करो, कर्म-कर्म, त्वम् तुम, कर्म-कर्म, ज्यायः-श्रेष्ठतर, हि-क्योंकि, अकर्मणः-कर्म न करने की अपेक्षा, शरीरयात्रा-शरीर का निर्वाह, अपि-भी, च-और, ते-तुम्हारा, न-नहीं, प्रसिद्धयेत् सम्भव, अकर्मणः - बिना कर्म के।
अनुवाद : तुम अपने नियत कर्म करो; क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म करना अधिक अच्छा है। और फिर, बिना कर्म किये इस शरीर की यात्रा भी तो पूर्ण नहीं होती अर्थात् शरीर का निर्वाह करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है।
व्याख्या : नियत कर्म वह आवश्यक कर्तव्य है जिसका पालन करना मनुष्य का धर्म है। विहित कर्म न करने पर दोष होता है। विहित कर्मों का पालन करने से किसी परिणाम-विशेष की प्राप्ति नहीं होती और इसके पालन से पुण्य मिलता हो, ऐसा भी नहीं है।
जीवन-निर्वाह के लिए ही सबको अनेक स्वाभाविक और अनिवार्य कर्म करने पड़ते हैं। "मैं बिना कोई कर्म किये रह सकता हूँ", ऐसा कहना अज्ञान है।
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ।।९ ।।
शब्दार्थ : यज्ञार्थात् - यज्ञ के लिए, कर्मणः-कर्म का, अन्यत्र-अन्यथा, लोकः-संसार, अयम्-यह, कर्मबन्धनः-कर्मबन्धन, तदर्थम् - उसके लिए, कर्म-कर्म, कौन्तेय हे कुन्तिपुत्र, मुक्तसङ्गः- अनासक्त हो कर, समाचर-आचरण करो।
अनुवाद : यज्ञ के भाव से किये जाने वाले कर्मों को छोड़ कर अन्य सभी कर्म भवबन्धन में डालने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अनासक्त हो कर यज्ञ के रूप में अपना कर्म करो।
व्याख्या : शुद्ध भाव से किया गया कोई भी निष्काम और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ कहलाता है। वेद की तैत्तिरीय संहिता में विहित है : "यज्ञो वै विष्णु"-"यज्ञ ही विष्णु है''(१.७.४)। भगवान् के लिए किया गया कोई भी कर्म बन्धन से मुक्त करने वाला है। विष्णु के निमित्त कर्म करने से मन निर्मल होता है। इस भाव का अभाव होने पर कर्म संसार-बन्धन में डालने वाला हो जाता है, वह कर्म अच्छा हो या बुरा। शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म बन्धन के कारण हैं। (निरूपण-ІІ.48)
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ।।१०।।
शब्दार्थ : सहयज्ञाः -यज्ञों सहित, प्रजा:-मनुष्यों को, सृष्ट्वा उत्पन्न करके, पुरा-पूर्वकाल में, उवाच-कहा, प्रजापतिः-प्रजापति ने, अनेन-इसके द्वारा, प्रसविष्यध्वम् सन्तान वृद्धि करो, एषः यह, वः तुम्हारी, अस्तु हो, इष्टकामधुक् - अभीष्ट-सिद्धि वाली कामधेनु ।
अनुवाद : (सृष्टि के) आदि काल में प्रजापति ने मनुष्यों को यज्ञ सहित उत्पन्न करके कहा- "इसके द्वारा तुम फलो, फूलो। सन्तान वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारे लिए समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु स्वरूप होगा।"
व्याख्या : प्रजापति सृष्टिकर्ता (ब्रह्मा) हैं। कामधुक्, कामधेनु का ही दूसरा नाम है। कामधेनु इन्द्र की गाय है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभीष्ट इच्छा की पूर्ति कर सकता है। (निरूपण - VIII.4; IX.24, 27; X.25)
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।।११ ।।
शब्दार्थ : देवान् -देवताओं को, भावयत-पोषण करो, अनेन-इसके द्वारा, ते वे, देवाः देव, भावयन्तु-पोषण करें, वः तुम्हारा, परस्परम् -एक-दूसरे का, भावयन्तः-पोषण करते हुए, श्रेयः-कल्याण, परम् सर्वोच्च, अवाप्स्यथ-प्राप्त करो।
अनुवाद : इसके द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो और वे देव तुम्हारा पोषण करें। इस प्रकार परस्पर, एक-दूसरे का सम्पोषण करते हुए तुम सर्वोच्च कल्याण को प्राप्त करोगे।
व्याख्या : देव का अर्थ है-दिव्य, ज्योतिर्मय । इस यज्ञ से तुम इन्द्र आदि देवताओं को प्रसन्न करो और देव गण वर्षा आदि के द्वारा तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। सर्वोच्च कल्याणप्रद तो भव-बन्धन से मुक्त करने वाला आत्म-ज्ञान है। स्वर्गलोक की प्राप्ति भी परम कल्याण से अभिहित हो सकती है। फल तो साधक की भावना पर निर्भर करता है।
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ।।१२ ।।
शब्दार्थ : इष्टान् -वांछित, भोगान् -पदार्थ, हि-निश्चित रूप से, वः-तुम्हें, देवाः देवगण, दास्यन्ते-देंगे, यज्ञभाविताः यज्ञ से प्रसन्न, तैः उनके द्वारा, दत्तान् दिये गये, अप्रदाय-बिना अर्पण (भेंट) किये, एभ्यः- उनके लिए, यः जो, भुङ्क्ते-भोग करता है, स्तेनः-चोर, एव-निश्चित रूप से, सः वह ।
अनुवाद : यज्ञ से प्रसन्न हो कर देव गण तुम्हें इच्छित पदार्थ प्रदान करेंगे। अतः उनके लिए अर्पण किये बिना जो मनुष्य उनके द्वारा प्रदत्त पदार्थों का भोग करता है, वह निश्चित रूप से चोर है।
व्याख्या : जब देवता तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, वे तुम पर सर्व सुख अर्थात् धन-ऐश्वर्य-समृद्धि, पशुधन और सन्तान आदि की वृष्टि करते हैं।
देवताओं द्वारा दिये गये भोगों को जो स्वयं भोगता है अर्थात् जो बदले में उन्हें अर्पित किये बिना अपने ही शरीर और इन्द्रियों की तृष्णाओं की पूर्ति करता है, वह निस्सन्देह चोर है। वह तो देवों की सम्पत्ति का डाकू है।
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ।।१३ ।।
शब्दार्थ : यज्ञशिष्टाशिनः - यज्ञ के अवशेष का भोग करने वाले, सन्तः सन्त, मुच्यन्ते-मुक्त हो जाते हैं, सर्वकिल्बिषैः-सब पापों से, भुञ्जते-उपभोग करते हैं, ते-वे, तु-निश्चय से, अघम् -पाप, पापा:-पापी जन, ये-जो, पचन्ति-पकाते हैं, आत्मकारणात्-अपने लिए।
अनुवाद : यज्ञावशेष का उपभोग करने वाले सन्त जन सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं; किन्तु जो पापी जन केवल अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप खाते हैं।
व्याख्या : पञ्चमहायज्ञ करने के उपरान्त जो मनुष्य यज्ञावशेष का उपभोग करते हैं, वे इन पाँच प्रकार के पापों से बच जाते हैं जो पाप ज्ञान-अज्ञान में पाँच प्रकार के कीट आदि की हिंसा से लगते हैं, वे हैं- (१) ओखल-मूसल, (२) चक्की, (३) 37sqrt(17) -स्थान, (४) वह स्थान जहाँ पेय जल रखा जाता है, (५) झाडू का स्थान। ये पाँच स्थान हैं, जहाँ प्रतिदिन जीवन-हिंसा होती ही है। पंच महायज्ञों के अनुष्ठान से ये पाप क्षीण हो जाते हैं। प्रत्येक द्विज (हिन्दू संस्कृति के अनुसार प्रथम तीन वर्ण, विशेषकर ब्राह्मण) को ये यज्ञ अवश्य करने चाहिए।
(१) देव-यज्ञ-देव गणों के लिए यज्ञ में आहुति देना जो उन्हें सन्तुष्ट करेगी।
(२) ब्रह्म-यज्ञ अथवा ऋषि-यज्ञ-ऋषियों और ब्रह्म को सन्तुष्ट करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन।
(३) पितृ-यज्ञ-पितरों को सन्तुष्ट करने हेतु उन्हें जल की आहुति (अर्घ्य) देना ।
(४) नृ-यज्ञ (अतिथि-यज्ञ) - अतिथि और भूखे को भोजन कराना।
(५) भूत-यज्ञ-पशु-पक्षियों को भोजन देना ।
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।।१४।।
शब्दार्थ : अन्नात् -अन्न से, भवन्ति - (उत्पन्न) होते हैं, भूतानि-भौतिक प्राणी, पर्जन्यात् वर्षा से, अन्नसम्भवः-अन्न की उत्पत्ति, यज्ञात्-यज्ञ से, भवति -होती है, पर्जन्यः- वृष्टि, यज्ञः -यज्ञ, कर्मसमुद्भवः-कर्म से उत्पन्न ।
अनुवाद : अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है। वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है।
व्याख्या : यहाँ यज्ञ का अर्थ है-अपूर्व अथवा सूक्ष्म तत्त्व अथवा अव्यक्त स्वरूप जो परिणाम की अभिव्यक्ति और अनुष्ठान के मध्यकाल में यज्ञ धारण करता है। (कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान के समय अथवा परिणाम काल में जो अदृश्य रूप धारण करता है, वह अपूर्व है।)
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।।१५ ।।
शब्दार्थ : कर्म-कर्म, ब्रह्मोद्भवम् - ब्रह्म से उत्पन्न, विद्धि-जानो, ब्रह्म-ब्रह्म, अक्षरसमुद्भवम् - अक्षर सर्वगतम् सर्वव्यापक, ब्रह्म-ब्रह्म, प्रतिष्ठितम् - विद्यमान रहता है। से उत्पन्न, तस्मात् - इसलिए, नित्यम् -सदा, यज्ञे-यज्ञ में,
अनुवाद : यह जान लो कि कर्म का उद्भव ब्रह्म से है और ब्रह्म अक्षर (अनश्वर) से उद्भूत है। अतः सर्वव्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता है।
व्याख्या : ब्रह्म का अर्थ है-वेद। जिस प्रकार श्वास मनुष्य के मुख से निकसित होता है, उसी प्रकार वेद अविनाशी, सर्वज्ञ परमात्मा का श्वास है। वेद सदा यज्ञ में विद्यमान रहता है अर्थात् मुख्यतः यह यज्ञ और उसके अनुष्ठान के विधि-विधान का निरूपण करता है। (निरूपण - IV. 24 से 32)
कर्म-कर्म, ब्रह्मोद्भवम् वेदों के आदेशों से उत्पन्न ।
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ।।१६ ।।
शब्दार्थ : एवम् - इस प्रकार, प्रवर्तितम् -घुमाये जाते हुए, चक्रम् -चक्र का, न-नहीं, अनुवर्तयति - अनुसरण करता है, इह-यहाँ, यः जो, अघायुः-पापी, इन्द्रियारामः - इन्द्रियों में रमण करने वाला, मोघम् - व्यर्थ ही, पार्थ पार्थ, सः वह, जीवति-जीता है।
अनुवाद : हे पार्थ, जो मनुष्य इस प्रवर्तित सृष्टिचक्र के अनुकूल व्यवहार नहीं करता, वह इन्द्रियों में रमण करने वाला व्यर्थ ही जीता है।
व्याख्या : यह कर्म का चक्र है जिसे यज्ञ और वेद के आधार पर सृष्टिकर्ता ने गति प्रदान की है। उसका जीवन व्यर्थ है जो यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म और वेद-विहित आदेश का पालन न करते हुए ऐन्द्रिक विषयों में लिप्त रहता है। वह अपना जीवन ही व्यर्थ गँवा रहा है। वस्तुतः वह निरर्थक जीवन व्यतीत कर रहा है।
जो भी व्यक्ति इस नियम का अनुसरण नहीं करता और स्वार्थी है, वह मानो पाप-कर्म कमा रहा है। परमात्मा के नियम के विरुद्ध चलना सबसे बड़ा अपराध है।
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।।१७ ।।
शब्दार्थ : यः-जो, तु-किन्तु, आत्मरतिः- आत्मा में आनन्द लेने वाला, एव-ही, स्यात् -हो, आत्मतृप्तः- आत्मा में सन्तुष्ट, च-और, मानवः मनुष्य, आत्मनि-आत्मा में, एव-ही, च-और, सन्तुष्टः सन्तुष्ट, तस्य-उसका, कार्यम् कार्य, न-नहीं, विद्यते- है।
अनुवाद : किन्तु उस मनुष्य के लिए कोई और कर्तव्य करने को शशेष नहीं रहता जो आत्मा में सन्तुष्ट है, आत्मा से तृप्त है और आत्मा में ही आनन्द की अनुभूति करता है।
व्याख्या : सुख-प्राप्ति हेतु ज्ञानी या मुनि बाह्य विषयों पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने में ही सन्तुष्ट रहता है, अपनी ही आत्मा में वह सुख, सन्तोष और आनन्द की खोज करता है। ऐसे योगी के लिए, जिसे आत्म-ज्ञान हो गया है, कुछ अन्य कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। वह कर्मभाव से मुक्त हो कर, कर्म की पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। वह आप्तकाम है, पूर्णतया आत्म-सन्तुष्ट है। (निरूपण -11.55)
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ।।१८ ।।
शब्दार्थ : न -नहीं , एव-ही, तस्य-उसके, कृतेन-कर्म से, अर्थ:- अभिप्राय, ननहीं, अकृतेन-कर्म न करने से, इह-यहाँ, कश्चन-कोई, न-नहीं, च-और, अस्य-इसका, सर्वभूतेषु सब प्राणियों में, कश्चित् -कोई, अर्थव्यपाश्रयः विषय पर निर्भरता।
अनुवाद : ऐसे महान् पुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने का ही कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने का। वह किसी विषय के लिए किसी प्राणी पर निर्भर नहीं रहता।
व्याख्या : एवंविध, आत्मा में ही सन्तुष्ट महात्मा को कर्म से कोई प्रयोजन नहीं रहता । कर्म से उसका वस्तुतः कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। अकर्म से उसको प्रत्यवाय दोष छू भी नहीं सकता। कर्म न करने से उसे कोई हानि नहीं होती। वस्तु-विशेष की प्राप्ति हेतु उसे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। न ही किसी प्राणी का अनुग्रह उसे चाहिए।
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।।१९ ।।
शब्दार्थ : तस्मात् - इसलिए, असक्तः - बिना आसक्ति, सततम् -निरन्तर, कार्यम् -कर्तव्य कर्म, कर्म-कर्म, समाचर-करो, असक्तः - बिना आसक्ति, हि-क्योंकि, आचरन् करते हुए, कर्म-कर्म, परम् - परमात्मा को, आप्नोति-प्राप्त करता है, पूरुषः-पुरुष ।
अनुवाद : इसलिए आसक्ति रहित हो कर तुम कर्तव्य कर्म को करो; क्योंकि आसक्ति का त्याग कर के कर्म करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है।
व्याख्या : आसक्ति रहित हो कर यदि तुम भगवदर्थ (भगवान् के लिए) कर्म करोगे, तो हृदय की शुचिता से आत्म-साक्षात्कार करोगे। (निरूपण- II.64, IV.19, 23; XVIII.49)
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ।।२० ।।
शब्दार्थ : कर्मणा-कर्म के द्वारा, एव-ही, हि-निश्चय से, संसिद्धिम् पूर्णत्व, आस्थिताः- प्राप्त किया, जनकादयः- जनकादि ने, लोकसंग्रहम् लोककल्याण, एव-ही, अपि-भी, संपश्यन् - देखते हुए, कर्तुम् -करने के लिए, अर्हसि योग्य हो।
अनुवाद : जनक तथा अन्य लोग निश्चित रूप से कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त कर सके। लोकसंग्रह अर्थात् सामान्य जनों का पथ-प्रदर्शन करने के दृष्टिकोण से भी तुम्हें कर्म करना चाहिए।
व्याख्या : संसिद्धि का अर्थ है मोक्ष । जनक, अश्वपति तथा अन्य राजाओं को आत्मा का पूर्ण ज्ञान था। पुनरपि जनगण के समक्ष उदाहरण रखने के लिए उन्होंने कर्म किया। लोगों को मार्ग-दर्शन कराने के लिए उन्होंने कर्म किया।
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।२१ ।।
शब्दार्थ : यद्यत्-जो-जो, आचरति-आचरण करता है, श्रेष्ठः - श्रेष्ठ मनुष्य, तत्-तत्-वही-वही, एव-ही, इतरः-अन्य, जनः लोग, सः वह (महापुरुष), यत्-जो, प्रमाणम् - आदर्श उपस्थित करना, कुरुते-करता है, लोकः संसार (लोग), तत्-उसका, अनुवर्तते-अनुसरण करता है।
अनुवाद : श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा करते हैं। वे जो प्रमाणित कर देते हैं अर्थात् जो भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं, अन्य लोग उसका अनुगमन करते हैं।
व्याख्या : मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अनुकारक भी है। अपने शुभ-अशुभ विचारों का निर्णय वह उनसे लेता है जो नैतिकता में उससे श्रेष्ठतर हैं। जैसा आचरण एक महापुरुष करता है, उसके अनुयायी उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। उसके चरणचिह्नों का अनुसरण उनका प्रयत्न होता है।
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ।। २२ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, मे-मेरे लिए, पार्थ-पार्थ (अर्जुन), अस्ति-है, कर्तव्यम् -करने योग्य कर्म, त्रिषु लोकेषु-तीनों लोकों में, किश्चन-कुछ भी, न-नहीं, अनवाप्तम् - अप्राप्त, अवाप्तव्यम् -प्रापणीय, वर्ते-लगा रहता हूँ, एव-ही, चऔर, कर्मणि-कर्म में।
अनुवाद : हे अर्जुन, तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य है और न ही ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे अप्राप्त हो और प्राप्त करनी हो । पुनरपि मैं स्वयं को कर्म में संलग्न रखता हूँ।
व्याख्या : मैं विश्व-नियन्ता हूँ; इसलिए व्यक्तिगत क्षेत्र में मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है; क्योंकि मेरे पास दैवी सम्पदा है, समस्त ब्रह्माण्ड का ऐश्वर्य मेरे पास है, फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ।
तुम मेरा अनुसरण क्यों नहीं करते? अपना दृष्टान्त दूसरों के समक्ष रख कर तुम सामान्य लोगों को अनुचित मार्ग पर चलने से रोकने का साहस क्यों नहीं करते ? तुम यदि कोई आदर्श स्थापित करोगे, तो लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे; क्योंकि तब तुम सद्गुण-सम्पन्न एक अग्रणी नेता बन जाओगे ।
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।
मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।२३ ।।
शब्दार्थ : यदि-यदि, हि-निश्चित रूप से, अहम् मैं, न -नहीं, वर्तेयम् - (कर्म में) व्यस्त रहूँ, जातु-कभी, कर्मणि-कर्म में, अतन्द्रितः-निरालस्य, मम-मेरे, वत्र्म-पथ, अनुवर्तन्ते-अनुसरण करते हैं, मनुष्याः- लोग, पार्थ- पार्थ, सर्वशः -सब प्रकार से।
अनुवाद : हे अर्जुन, यदि मैं सावधान हो कर कर्म में व्यस्त न रहूँ, तो सब मनुष्य भी सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे।
व्याख्या : यदि मैं आलसी (अकर्मी) हो जाऊँ, तो सब लोग मेरा अनुवर्तन कर के मौन बैठ जायेंगे। वे तामसिक हो कर जड़ता को प्राप्त करेंगे।
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ।
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ।।२४ ।।
शब्दार्थ : उत्सीदेयुः नष्ट हो जायें, इमे-ये, लोकाः लोक, ननहीं, कुर्याम् -करूँ, कर्म-कर्म, चेत्-यदि, अहम् - मैं, संकरस्य-जातियों के अन्तर्मिश्रण का, च-और, कर्ता-बनाने वाला, स्याम् - बनूँ, उपहन्याम् नष्ट करूँ, इमाः ये सब, प्रजाः प्राणी।
अनुवाद : यदि मैं कर्म न करूँ, तो इस संसार को नष्ट करने वाला बनूँ। संकर (अव्यवस्था) को उत्पन्न करने वाला और प्रजा का हनन करने वाला बन जाऊँ।
व्याख्या : यदि मैं कर्म में निरत न होता, तो लोक भी निष्क्रिय हो जाते। वे वर्णाश्रम धर्म का पालन न करते जो उन्हें अपने-अपने जीवन की चार अवस्थाओं में क्रमशः करना होता । अतः जाति भ्रम उत्पन्न होता और मुझे उन्हें नष्ट करना पड़ता ।
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ।।२५ ।।
शब्दार्थ : सक्ताः- आसक्त, कर्मणि-कर्म में, अविद्वांसः-अज्ञानी, यथा-जैसे, कुर्वन्ति-करते हैं, भारत-हे भारत, कुर्यात् -करे, विद्वान् -विद्वान्, तथा वैसे, असक्तः अनासक्त, लोकसंग्रहम्-लोककल्याण की । चिकीर्षुः कामना करते हुए,
अनुवाद : हे भारत (अर्जुन), जिस प्रकार से एक अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त हो कर कर्म करता है उसी प्रकार से एक विद्वान् पुरुष लोककल्याणार्थ आसक्तिरहित हो कर कर्म करे।
व्याख्या : फल की कामना से अविद्वान् कार्य करता है। वह कहता है-"अमुक कार्य करके मैं अमुक फल की प्राप्ति करूँगा"; किन्तु विद्वान् पुरुष जो आत्मज्ञानी है, अपने लिए कर्म नहीं करता। उसे तो ऐसा कर्म करना चाहिए कि वह दूसरों के लिए दृष्टान्त बन जाये और लोग उससे शान्ति, समन्वय, हृदय की शुचिता, दिव्य प्रकाश और ज्ञान प्राप्त करें। आत्मज्ञानी ही विद्वान् है। (निरूपण - II 64; III 19; XVIII.49)
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ।। २६ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, बुद्धिभेदम् -मन का विचलित होना, जनयेत्-उत्पत्र करे, अज्ञानाम् अज्ञानियों के, कर्मसङ्गिनाम् -कर्म में आसक्त मनुष्यों के जोषयेत् लगाये, सर्वकर्माणि-सब कर्म, विद्वान् बुद्धिमान्, युक्तः - युक्त- समाचरन् आचरण करते हुए।
अनुवाद : विद्वान् पुरुष को चाहिए कि वह कर्म में आसक्त अज्ञान व्यक्तियों के मन को विचलित न करे। स्वयं भक्तिभाव से परिपूर्ण हो कर वह युक्त पुरुष दूसरों को सभी कर्मों के करने में प्रेरणा दे।
व्याख्या : एक अज्ञानी मनुष्य स्वयं से कहता है- "मैं यह काम करूँगा और इसका फल भोगूँगा।" विद्वान् मनुष्य उसके विश्वास को न तोड़े उससे अपेक्षा यही है कि वह अनासक्त भाव से कर्म कर के उसके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करे। उसे चाहिए कि वह अज्ञानी को अनुशासित करे और उसे कर्म की उपेक्षा न करने का ज्ञान दे। आवश्यकता पड़ने पर उसे इस प्रकार (अनास कर्म) से प्राप्त सुख के इस लोक और परलोक के विविध रङ्ग बताये। समय साथ हृदय पवित्र होने पर विद्वान् उनमें निष्काम कर्मयोग के बीज बो सकता है।
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ।।२७ ।।
शब्दार्थ : प्रकृतेः-प्रकृति के, क्रियमाणानि-किये जा रहे, गुणैःगु के द्वारा, कर्माणि-कर्म, सर्वशः-सब प्रकार से, अहंकारविमूढात्मा-अहंकार भ्रमित (मोहित) मन वाला, कर्ता-करने वाला, अहम् -मैं, इति-ऐस मन्यते मानता है।
अनुवाद : सभी प्रकार से समस्त कर्म वस्तुतः प्रकृति के गुणों से सम् होते हैं; किन्तु अहंभाव से मोहित अथवा मूढ़ हुआ व्यक्ति स्वयं को ही क मान बैठता है।
व्याख्या : प्रकृति अथवा प्रधान वह अवस्था और तमस्-ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। इस साम्यावस्था के है जिसमें सत्त्व, रजस् असन्तुलन से सृष्टि प्रारम्भ होती है। शरीर, मन, इन्द्रियाँ आदि बनते हैं। अहंकार से भ्रमित व्यक्ति शरीर, मन, इन्द्रियों और प्राण का आत्मा के साथ एकत्व मानने लगता है और शरीर तथा इन्द्रियों की उपाधि का आत्मा में अध्यारोपण (निक्षेप) करता है। अतः अज्ञानवश वह सोचता है- “मैं कर्ता हूँ।" वस्तुतः प्रकृति के गुण ही सब कर्म करते हैं। (निरूपण - III.29; V.9; IX.9, 10; XIII.21, 24, 30, 32; XVIII.13, 14)
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।।२८ ।।
शब्दार्थ : तत्त्ववित् सत्य को जानने वाला, तु-लेकिन, महाबाहो-हे महाबाहु (अर्जुन), गुणकर्मविभागयोः- गुण और कर्म के विभाग के, गुणाः गुण (इन्द्रियों के रूप में), गुणेषु गुणों में, वर्तन्ते-रहते हैं, इति-ऐसा, मत्वा-मान कर, न-नहीं, सज्जते आसक्त होता है।
अनुवाद : किन्तु हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, गुण और कर्मविभाग के तत्त्व को जानने वाला तत्त्वविद्, गुण (इन्द्रियाँ) गुणों (विषयों) में ही बरत रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ऐसा जान कर उनमें आसक्त नहीं होता।
व्याख्या : आत्मा तीन गुणों और कर्मों से सर्वथा पृथक् है, इस तत्त्व को जानने वाला कर्म में आसक्त नहीं होता। गुण-विभाग और कर्म-विभाग का मर्म जान लेने के पश्चात् (गुण-कर्म के अन्योन्य क्रियाकलाप जानने के पश्चात्) ज्ञानी भलीभाँति समझ लेता है कि गुण स्वरूप इन्द्रियाँ गुण रूप विषयों में विचरण करती हैं। अतः उसकी कर्म में आसक्ति नहीं होती। वह जानता है-“मैं अकर्ता हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ"। (निरूपण-XIV.23)
प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत् ।।२९ ।।
शब्दार्थ : प्रकृतेः - प्रकृति के, गुणसम्मूढाः गुणों से मोहित, सज्जन्ते-आसक्त होते हैं, गुणकर्मसु गुणों के कार्यों में, तान्-उन, अकृत्स्नविदः-अल्प ज्ञानी, मन्दान् -मूढ़, कृत्स्नवित्-पूर्ण ज्ञानी, न-नहीं, विचालयेत् - विचलित न करे।
अनुवाद : प्रकृति के गुणों के कारण सम्भ्रान्त व्यक्ति उन गुणों से उत्पन्न कर्मों में आसक्त होते हैं। एक ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह उन मूढ़ व्यक्तियों को विचलित न करे जो अल्प ज्ञान वाले हैं अथवा जो प्रकृति की प्रेरणा से सकाम कर्म करते हैं।
व्याख्या : अज्ञानी लोग फल की आकाङ्क्षा से कर्म करते हैं; किन्तु आत्मा का ज्ञान रखने वाले बुद्धिमान् पुरुष से यह अपेक्षित है कि वह अज्ञानी व्यक्तियों के श्रद्धा, विश्वास और विचारधारा को विचलित न करे, क्योंकि ऐसा करने से वे (अज्ञानी व्यक्ति) कर्म को त्याग कर तमस् का शिकार हो जायेंगे। वे आलसी, निष्प्रयोजन जीवन यापन करेंगे। प्रारम्भ में उन्हें सकाम कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए। धीरे-धीरे ज्ञानी पुरुष उन्हें निष्काम कर्मयोग में प्रवृत्त करें, उन्हें इच्छा रहित कर्म के लाभों से अवगत करायें जैसे आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाने वाली हृदय की पवित्रता ।
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।। ३० ।।
शब्दार्थ : मयि-मुझ में, सर्वाणि-सब, कर्माणि-कर्म, संन्यस्य-त्याग कर, अध्यात्मचेतसा आत्म-केन्द्रित मन से, निराशी:- निष्काम भाव से, निर्ममः- अहंकारशून्य, भूत्वा हो कर, युध्यस्व-युद्ध करो, विगतज्वरः- उद्वेग रहित हो कर ।
अनुवाद : समस्त कर्म मुझे समर्पित कर के, चेतना को आत्मा में स्थिर कर के, आशा (इच्छा) और अहंकारशून्य हो कर, निरुद्वेग हो कर तुम युद्ध करो।
व्याख्या : समस्त कर्म मेरे अर्पण कर दो। “मैं सब कर्म भगवान् के लिए करता हूँ", ऐसा चिन्तन करो।
ज्वर का अर्थ है-दुःख, सन्ताप । (निरूपण - V.10; XVIII.66)
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ।।३१ ।।
शब्दार्थ : ये जो, मे मेरी, मतम् -शिक्षा, इदम्-इस, नित्यम् -सदा, अनुतिष्ठन्ति-अभ्यास (अनुपालन) करते हैं, मानवाः मनुष्य, श्रद्धावन्तः श्रद्धापूर्ण हो कर, अनसूयन्त:-ईर्ष्या रहित हो कर, मुच्यन्ते-मुक्त हो जाते हैं, ते-वे, अपि-भी, कर्मभिः कर्मों से।
अनुवाद : स्पृहा रहित हो कर, श्रद्धा युक्त हो कर जो मनुष्य नित्य मेरे इस उपदेश का अनुपालन करते हैं, वे कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाते हैं।
व्याख्या : श्रद्धा, एक मानसिक वृत्ति है, विश्वास के अर्थ में। यह विश्वास है अपनी आत्मा में, शास्त्रों में और आध्यात्मिक गुरु के उपदेशों में। यह श्रद्धा, सम्मान और नम्रता का उच्च भाव में सम्मिश्रण है।
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ।।३२ ।।
शब्दार्थ : ये-जो, तु-किन्तु, एतत् - यह, अभ्यसूयन्तः- दोषदृष्टि रखते हुए, न-नहीं, अनुतिष्ठन्ति-अभ्यास करते हैं, मे-मेरे, मतम् उपदेश, सर्वज्ञानविमूढान् सब ज्ञान के प्रति मूढ़ (भ्रमित), तान् उन्हें, विद्धि-जानो, नष्टान् नष्ट हुए, अचेतसः - विवेकशून्य ।
अनुवाद : किन्तु वे लोग जो मेरे उपदेशों में दोषदृष्टि रखते हैं और उनका पालन नहीं करते, ऐसे विवेकशून्य और सभी प्रकार के ज्ञान में भ्रमित लोगों को नष्ट हुआ जानो अर्थात् उनका विनाश अपरिहार्य है।
व्याख्या : दुराग्रही और स्थूलधी मनुष्य जो भगवान् के उपदेशों में दोषदृष्टि रखते हैं और उनकी शिक्षाओं को आचरण में नहीं लाते, निश्चित रूप से विनाश के अधिकारी हैं। वे अशोच्य हैं, शिक्षातीत हैं और वास्तव में मूढ़ ही हैं।
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्शानवानपि ।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।। ३३ ।।
शब्दार्थ : सदृशम् अनुसार (अनुरूप), चेष्टते-चेष्टा करता है, स्वस्याः-अपने, प्रकृतेः-प्रकृति (स्वभाव) के, ज्ञानवान् बुद्धिमान्, अपि-भी, प्रकृतिम् - प्रकृति को, यान्ति-अनुसरण करते हैं, भूतानि-प्राणी, निग्रहः संयम, किम् -क्या, करिष्यति-करेगा ।
अनुवाद : एक ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वभाव के अनुरूप चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के वशीभूत हो कर ही कार्य करते हैं। इसमें निग्रह (संयम) क्या करेगा?
व्याख्या : इस श्लोक को पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है मानो मनुष्य के व्यक्तिगत प्रयास का कोई आशय ही नहीं है। किन्तु ऐसा नहीं है। निम्न श्लोक पढ़ो। इसमें स्पष्ट संकेत है कि राग-द्वेष से ऊपर उठ कर मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है।
एक अज्ञानी और मोहग्रस्त व्यक्ति ही अपनी निम्न प्रकृति और स्वाभाविक प्रवृत्तियों के प्रवाह में बहने लगता है। न तो उसे अपनी इन्द्रियों पर संयम है और न ही इच्छा-अनिच्छा की दो धाराओं पर । पुरुषार्थ चतुष्टय से समन्वित एक सत्यान्वेषक, जो सतत ध्यानाभ्यास में रत है, सहज रूप से अपनी प्रकृति को संयत कर सकता है। (निरूपण - II.60; V.14; XVIII.59)
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ।। ३४ ।।
शब्दार्थ : इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य-प्रत्येक इन्द्रिय के, अर्थ-विषय में, रागद्वेषौ राग और द्वेष, व्यवस्थितौ - स्थित हैं, तयोः-उन दोनों के, न-नहीं, वशम् वश में, आगच्छेत् - आना चाहिए, तौ-वे दोनों, हि-निश्चित रूप से, अस्य-इसके, परिपन्थिनौ-शत्रु हैं।
अनुवाद : ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग और द्वेष इन्द्रियों में ही समाया रहता है। अतः मनुष्य को इन दोनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए; क्योंकि वे इसके शत्रु हैं।
व्याख्या : सुखद विषय के लिए प्रत्येक इन्द्रिय का आकर्षण होता है और इसके विपरीत दुःखद अथवा प्रतिकूल विषय के प्रति इन्द्रिय का विकर्षण होता है। राग-द्वेष की वृत्तियों को संयत कर लेने पर, मनुष्य पर उनका प्रभाव नहीं रहता । यहाँ व्यक्तिगत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से स्वयं उद्भूत सुप्त वृत्तियाँ अथवा सम्पूर्ण संस्कार जो मनुष्य की प्रकृति (स्वभाव) के लिए उत्तरदायी हैं, मनुष्य को राग और द्वेष के दो वेगों से उसके मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। यदि कोई इन दो वेगों को वश में कर ले; विवेक, विचार और आत्मान्वेषण से प्रेम और घृणा से ऊपर उठ जाये, तो वह प्रकृति पर विजयी हो कर अमृतत्व और शाश्वत आनन्द का आनन्द ले सकता है। अब वह अपनी प्रकृति के अधिकार में नहीं होगा। अतः इन्द्रिय-विषयों में राग-द्वेष की भावना से स्वयं को मुक्त करने का उपाय करना चाहिए।
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।।३५ ।।
शब्दार्थ : श्रेयान् -श्रेष्ठ, स्वधर्मः - अपना धर्म (कर्तव्य), विगुणः गुण रहित, परधर्मात् -दूसरे के धर्म से, स्वनुष्ठितात्-भलीभाँति किये हुए, स्वधर्मे-अपने धर्म में, निधनम् -मृत्यु, श्रेयः-कल्याणप्रद, परधर्मः -दूसरे का धर्म, भयावहः भयप्रद ।
अनुवाद : भली प्रकार से पालन किये जा रहे दूसरे के धर्म की अपेक्षा अपना धर्म दोषयुक्त अथवा अपूर्ण रूप से पालन किया जा रहा भी श्रेयस्कर है। अपने धर्म के लिए मृत्यु (का वरण) भी कल्याणकारी है; किन्तु दूसरे का धर्म भय प्रदान करने वाला है।
व्याख्या : दूसरे के धर्म का उत्कृष्ट रूप से पालन करते हुए जीवित रहने की अपेक्षा दोषयुक्त अपने धर्म के लिए प्राण त्यागना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। दूसरे के धर्म में भय बना रहता है (वह मानो अन्धकूप है) । क्षत्रिय का धर्म (कर्तव्य) न्यायपरायण युद्ध करना है। अर्जुन को युद्ध करना ही है। यह उसका धर्म है। अपने धर्म को निभाते हुए वह प्राणों से हाथ भी धो बैठे, तो उसके लिए यही कल्याणकारी है। वह स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। उसे किसी अन्य धर्म का पालन उचित नहीं है। इससे उसके अन्तर्मन में शंका उत्पन्न होगी। युद्ध को त्याग कर संन्यास-मार्ग का वरण उसके लिए हितकर नहीं है। (निरूपण-XVIII.47)
अर्जुन उवाच
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।
अनिच्छन्नपि वार्णेय बलादिव नियोजितः ।।३६ ।।
शब्दार्थ : अथ-अब, केन-किसके द्वारा, प्रयुक्तः -प्रेरित हो कर, अयम् - यह, पापम् -पाप, चरति-करता है, पूरुषः- मनुष्य, अनिच्छन् - इच्छा न होते हुए, अपि भी, वाष्र्णेय-हे वाष्र्णेय (कृष्ण), बलात् -हठपूर्वक, इव-मानो, नियोजितः- नियुक्त ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे कृष्ण, इच्छा के विरुद्ध मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए कौन प्रेरित करता है, मानो उससे बलपूर्वक करवाया जा रहा हो ?
व्याख्या : वृष्णि वंश में उत्पन्न वार्णेय कहलाता है। यह भगवान् कृष्ण का एक नाम है।
श्री भगवानुवाच
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम् ।। ३७ ।।
शब्दार्थ : कामः इच्छा, एषः- यह, क्रोधः क्रोध, एषः- यह, रजोगुणसमुद्भवः रजोगुण से उत्पन्न, महाशनः सर्वभक्षक, महापाप्मा-महापापी, विद्धि-जानो, एनम् -इसे, इह-यहाँ, वैरिणम्-शत्रु ।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : रजोगुण से उत्पन्न यह क्रोध और इच्छा ही सर्वभक्षक और सर्वपापमय हैं। इस लोक में इन्हें ही शत्रु मानो ।
व्याख्या : भगवान्-भग शब्द छह उपाधियों से युक्त है, वे हैं-ज्ञान, वैराग्य, कीर्ति, ऐश्वर्य, श्री और बल। इन छह गुणों से युक्त पुरुष, जिसे सृष्टि के आदि और अन्त का भी ज्ञान है 'भगवान्' संज्ञा से विहित है।
इस संसार में पाप और दुष्कर्म की जननि इच्छा है। क्रोध इच्छा का ही मूर्त रूप है। इच्छापूर्ति में बाधा डालने वालों के प्रति मनुष्य क्रोधित होता है, जब उसकी इच्छा अपूर्ण रह जाती है। इच्छा रजोगुण से उत्पन्न है। इच्छा उत्पन्न होने पर रजोगुण अंकुरित होता है जो मनुष्य को वस्तु-विशेष की प्राप्ति हेतु कर्म में प्रेरित करता है। अतः यह जान लो कि इस धरा पर इच्छा ही मनुष्य की शत्रु है। (निरूपण-XVI.21)
धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाऽऽदर्शो मलेन च ।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ।।३८ ।।
शब्दार्थ : धूमेन धुएँ से, आव्रियते-ढक जाता है, वह्निः- अग्नि, यथा-जैसे, आदर्शः दर्पण, मलेन -धूल से, च-और, यथा-जैसे, उल्बेन-ज़ेर से, आवृतः ढका रहता है, गर्भः- गर्भ, तथा-उसी प्रकार, तेन-उसके द्वारा, इदम् - यह, आवृतम् ढका है।
अनुवाद : जिस प्रकार अग्नि धुएँ से, दर्पण धूल से और गर्भ ज़ेर से ढके रहते हैं, उसी प्रकार यह (ज्ञान) उससे (रजोगुण से) ढका रहता है।
व्याख्या : 'इदम्' का अभिप्राय ब्रह्माण्ड अथवा ज्ञान से है और 'तेन' का प्रयोग रजोगुण (इच्छा) के लिए हुआ है।
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ।। ३९ ।।
शब्दार्थ : आवृतम् -ढका हुआ है, ज्ञानम्-ज्ञान, एतेन-इसके द्वारा, ज्ञानिनः- ज्ञानियों का, नित्यवैरिणा - चिरशत्रु से, कामरूपेण-कामरूप, कौन्तेय-हे कुन्तीपुत्र, दुष्पूरेण-कभी शान्त न होने वाली, अनलेन-आग के द्वारा, च- और।
अनुवाद : हे अर्जुन, कभी शान्त न होने वाली अग्नि स्वरूप इच्छा से (जो कभी तृप्त नहीं होती) ज्ञानी का ज्ञान आवृत रहता है। यही उसकी चिरशत्रु है।
व्याख्या : मनु कहते हैं-विषय-भोग द्वारा इच्छाएँ न तो कभी पूर्ण होती हैं और न ही शान्त होती हैं। आग में घी और समिधा डालने पर जैसे वह और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, वैसे ही भोग्य-पदार्थों द्वारा इच्छा-पूर्ति करने पर तृष्णाएँ और अधिक जागृत होती हैं। धरती की समग्र भोग्य-सामग्री, समस्त अमूल्य धातुएँ, सारे पशु और सब सुन्दरियाँ यदि इच्छा करने वाले मनुष्य को उपलब्ध हो जायें, तब भी वे सब उसे सन्तोष नहीं दे सकते । तृष्णा जाग्रत होने पर अज्ञानी मनुष्य उसे अपना मित्र समझता है। इन्द्रियों की सन्तुष्टि हेतु वह इच्छाओं की पूर्ति करता है। किन्तु ज्ञानी मनुष्य परिणाम भोगने से पूर्व ही अनुभव से जान लेता है कि इच्छाएँ तो उसे दुःख और विपत्ति में डाल सकती हैं। अतः ज्ञानी के लिए तो ये नित्य वैरी के समान हैं और अज्ञानी के लिए मित्र हैं।
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ।।४० ।।
शब्दार्थ : इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ, मनः- मन, बुद्धिः बुद्धि, अस्य-इसका, अधिष्ठानम् वास-स्थान, उच्यते-कहा जाता है, एतैः- इनके द्वारा, विमोहयति-भ्रान्त करती है, एषः—यह, ज्ञानम्-ज्ञान को, आवृत्य ढक कर, देहिनम् - देहधारी (आत्मा को) ।
अनुवाद : इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इसके आधार (वास-स्थान) कहे गये हैं। इन्हीं के द्वारा यह (इच्छा) देहधारी के ज्ञान को आवृत करती है और उसे भ्रमित करती है।
व्याख्या : शत्रु के आश्रय-स्थल का ज्ञान हो जाये, तो उसे मारना सहज हो जाता है। एक बुद्धिमान् सेनानायक की भाँति भगवान् कृष्ण अर्जुन को इच्छाओं के आश्रय का संकेत देते हैं, जिससे वह उन पर आक्रमण कर अति-शीघ्र उनका विनाश कर सके।
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ।।४१ ।।
शब्दार्थ : तस्मात् - इसलिए, त्वम्-तुम, इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को, आदौ-आरम्भ में, नियम्य-संयत कर के, भरतर्षभ - हे भरतश्रेष्ठ, पाप्मानम् -विनाशकारी, प्रजहि-मार डालो, हि-निश्चित रूप से, एनम्-इसे, ज्ञानविज्ञाननाशनम् - ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले ।
अनुवाद : अतः, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ (अर्जुन), पहले इन्द्रियों को वश में करो । तत्पश्चात् ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को मार डालो।
व्याख्या : शास्त्राध्ययन से प्राप्त ज्ञान, ज्ञान है। यह परोक्ष ज्ञान (indirect knowledge) है। विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान (direct knowledge) है जो व्यक्तिगत अनुभव आत्म-साक्षात्कार से प्राप्त होता है। इन्द्रियों को वशीभूत कर के इच्छा को मार डालो।
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ।।४२ ।।
शब्दार्थ : इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को, पराणि-श्रेष्ठतर, आहुः-कहते हैं, इन्द्रियेभ्यः इन्द्रियों से, परम्-श्रेष्ठ, मनः-मन, मनसः मन से, तु-किन्तु, परा-श्रेष्ठ, बुद्धिः बुद्धि, यः- जो, बुद्धेः बुद्धि की अपेक्षा, परतः -श्रेष्ठ, तु-किन्तु, सः- वह (आत्म-तत्त्व है)।
अनुवाद : कहा जाता है कि इन्द्रियाँ (शरीर से) श्रेष्ठ हैं, मन इन्द्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है; किन्तु बुद्धि से भी श्रेष्ठ वह (आत्मा) है।
व्याख्या : ससीम, बाह्य, स्थूल, भौतिक शरीर की अपेक्षा इन्द्रियाँ सूक्ष्म, आन्तरिक और क्रिया की विपुल क्षेत्र वाली होने के कारण अधिक श्रेष्ठ हैं। मन इन्द्रियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है; क्योंकि मन की सहायता के बिना स्वतन्त्र रूप से इन्द्रियाँ कुछ भी नहीं कर सकतीं। पाँचों इन्द्रियों के क्रियाकलाप मन के आधीन होते हैं। विवेक-शक्ति से सम्पन्न होने के कारण बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। सन्दिग्धावस्था में बुद्धि ही मन की सहायता करती है। साक्षी आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है; क्योंकि बुद्धि आत्मा से ही प्रकाश प्राप्त करती है।
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ।।४३ ।।
शब्दार्थ : एवम् - इस प्रकार, बुद्धेः- बुद्धि की अपेक्षा, परम् - श्रेष्ठ, बुद्ध्वा जान कर, संस्तभ्य-स्थिर कर के, आत्मानम् - आत्मा को, आत्मना-आत्मा से, जहि-मार डालो, शत्रुम्-शत्रु को, महाबाहो - हे महाबाहु, कामरूपम् इच्छा रूपी, दुरासदम् दुर्जेय ।
अनुवाद : एवंविध, हे अर्जुन, उसे जान कर, जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है और आत्मा से आत्मा को संयत कर के, हे महाबाहु, तुम दुर्जेय काम रूपी शत्रु को जीत लो।
व्याख्या : निम्न आत्मा को उच्च आत्मा से वश में करो। निम्न मन को उच्च मन से जीत लो। काम को जीतना दुष्कर है, क्योंकि यह अत्यन्त जटिल और दुर्जेय है; किन्तु सतत घोर साधना में रत विवेकी और अनासक्त व्यक्ति इसे सुगमता से जीत सकता है। काम रजस् का गुण है। यदि तुम अपने भीतर सत्त्व गुण की वृद्धि करो, तो काम पर विजय प्राप्त कर सकते हो। सत्त्व के समक्ष रजस् नहीं टिक सकता। यद्यपि काम को जीतना कठिन है; परन्तु असम्भव कदापि नहीं है। इसकी सहज और सरल विधि है-जप और प्रार्थना द्वारा अन्तर्यामी परमात्मा से विनय करना।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ।।
।। इति कर्मयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ चतुर्थोऽध्यायः
ज्ञानविभागयोगः
श्री भगवानुवाच
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ।।१ ।।
शब्दार्थ : इमम्-इस, विवस्वते-विवस्वान् (सूर्यदेव) के लिए, योगम् योग को, प्रोक्तवान् -उपदेश दिया, अहम् -मैंने, अव्ययम् - अविनाशी, विवस्वान् - विवस्वान् ने, मनवे-मनु के लिए, प्राह-उपदेश दिया, मनुः मनु, इक्ष्वाकवे इक्ष्वाकु को, अब्रवीत् -कहा ।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : मैंने इस अविनाशी योग का ज्ञान विवस्वान् को दिया। विवस्वान् ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को इस योग का ज्ञान दिया।
व्याख्या : विवस्वान् सूर्य का पर्याय है। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे और वे सूर्यवंशी क्षत्रियों के पूर्वज थे।
योग अविनाशी कहा जाता है; क्योंकि इसका फल अर्थात् मोक्ष (योग से प्राप्त) अविनाशी है।
यदि राज्यों के शासक पिछले दो अध्यायों में उपदिष्ट योग का अनुसरण करें, तो वे राज्य को न्यायपूर्वक चला सकते हैं और ब्राह्मणों की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए सृष्टि के आदि काल में मैंने यह योग सूर्यदेव को सिखाया ।
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ।।२ ।।
शब्दार्थ : एवम् -इस प्रकार, परम्पराप्राप्तम्-परम्परा से प्राप्त, इमम् -इस (योग को), राजर्षयः राज-ऋषियों ने, विदुः -जाना, सः-वह, कालेन समय के साथ, इह-यहाँ, महता महान्, योग:- योग, नष्टः- नष्ट हो गया, परन्तप है परन्तप ।
अनुवाद : इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना । वही योग का ज्ञान हे अर्जुन, समय बीतने पर लुप्तप्राय-सा हो गया है।
व्याख्या : राजर्षि-राजा होते हुए ऋषि-पद को भी प्राप्त किया और इस योग को सीखा।
परन्तप-सूर्य की भाँति अपने पराक्रम और शक्ति से अर्जुन अपने शत्रु का विनाश करने में समर्थ था; इसलिए उसका नाम 'परन्तप' पड़ा।
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ।। ३ ।।
शब्दार्थ : सः-वह, एव-ही, अयम्-यह, मया-मेरे द्वारा, ते तुम्हारे लिए, अद्य-आज, योग: योग, प्रोक्तः-कहा गया, पुरातनः पुरातन, भक्तः - भक्त, असि-हो, मे-मेरे, सखा-मित्र, च-और, इति-इस प्रकार, रहस्यम् -रहस्य, हि-क्योंकि, एतत्-इस, उत्तमम् - श्रेष्ठ ।
अनुवाद : उसी पुरातन योग का ज्ञान आज मैंने तुम्हें दिया है; क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। यह (योग) एक परम रहस्य है।
व्याख्या : इस योग में सूक्ष्म और गहन उपदेश निहित हैं। अतः यह परम (श्रेष्ठ) रहस्य है जिसे भगवान् ने उद्घाटित किया ।
अर्जुन उवाच
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।।४।।
शब्दार्थ : अपरम् अर्वाचीन (पश्चात् काल का), भवतः - आपका, जन्म-जन्म, परम् -पूर्व, जन्म-जन्म, विवस्वतः-विवस्वान् का, कथम् -कैसे, एतत्-यह, विजानीयाम् समझ लूँ, त्वम्-आपने, आदौ-आदिकाल में, प्रोक्तवान् उपदेश किया, इति-इस प्रकार ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : आपका जन्म तो सूर्यदेव (विवस्वान्) के जन्म के पश्चात् हुआ। मैं कैसे यह मान लूँ कि आपने यह योग (सूर्य को) आदिकाल में दिया था।
व्याख्या : आपका जन्म तो उत्तरकाल में वसुदेव के घर में हुआ। विवस्वान् सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ। मैं कैसे मान जाऊँ कि प्रारम्भ में आपने यह विद्या सूर्यदेव को प्रदान की। और यह भी किस प्रकार जानूँ कि आपने जो सूर्य को विद्या दी, वही (भगवान्) मुझे आज यह विद्या दे रहे हैं। इसे समझना कठिन है। भगवन्, कृपा कर के मेरी इस जिज्ञासा को शान्त करें और सत्य को प्रकाशित करें।
श्री भगवानुवाच
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ।।५ ।।
शब्दार्थ : बहूनि बहुत, मे—मेरे, व्यतीतानि-बीत गये हैं, जन्मानि-जन्म, तव-तुम्हारे, च-और, अर्जुन-हे अर्जुन, तानि-उन सबको, अह्म - मैं , वेद-जानता हूँ, सर्वाणि-सब, न-नहीं, त्वम् -तुम, वेत्थ-जानते, परन्तप हे परन्तप ।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : हे परन्तप (अर्जुन), तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबका ज्ञान मुझे है; पर तुम्हें नहीं।
व्याख्या : तुम्हें अन्तर्ज्ञान (intuitional knowledge) नहीं है। तुम्हारे पूर्व कर्मोवश तुम्हारा दिव्य चक्षु अभी खुला नहीं है। इसलिए तुम्हारी दर्शन-शक्ति सीमित है और तुम्हें अपने पूर्व-जन्मों की स्मृति नहीं है। किन्तु मैं उन्हें जानता हूँ; क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ।
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।। ६ ।।
शब्दार्थ : अजः-अजन्मा, अपि-भी, सन् -होते हुए, अव्ययात्मा-अविनाशी प्रकृति का, भूतानाम् -प्राणियों का, ईश्वरः ईश्वर (स्वामी), अपि - भी, सन् -होते हुए, प्रकृतिम् -प्रकृति को, स्वाम्-अपनी, अधिष्ठाय-स्थित हो कर, संभवामि - प्रकट होता हूँ, आत्ममायया-अपनी माया से ।
अनुवाद : यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सब प्राणियों का स्वामी हूँ; पुनरपि अपनी प्रकृति में स्थित हो कर मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ।
व्याख्या : कर्म के बन्धन में आ कर मनुष्य जन्म धारण करता है। वह प्रकृति के वश में है। वह प्रकृति के तीन गुणों से भ्रमित है, जब कि भगवान् ने माया को पूर्णरूपेण अपने वश में कर रखा है। वे प्रकृति के शासक हैं; इसलिए वे प्रकृति के गुणों के आधीन नहीं हैं। माया-शक्ति के कारण यह आभास होता है कि उन्होंने जन्म लिया और शरीर धारण किया; किन्तु वास्तविकता कुछ और है। उनका शरीर धारण करना एक आविर्भाव (अभिव्यक्ति) है। उनकी सत्य प्रकृति अथवा दिव्यता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । (निरूपण-IX.8)
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ।।७ ।।
शब्दार्थ : यदा यदा-जब-जब, हि-निश्चित रूप से, धर्मस्य-धर्म की, ग्लानिः- हानि, भवति होती है, भारत- हे भारत, अभ्युत्थानम् - उत्थान (वृद्धि), अधर्मस्य अधर्म का, तदा-तब, आत्मानम् -स्वयं को, सृजामि-प्रकट करता हूँ, अहम् मैं।
अनुवाद : हे अर्जुन, (संसार में) जब-जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब-तब मैं प्रकट होता हूँ।
व्याख्या : धर्म, आलम्बन और संवर्धन दोनों एक ही बार में प्रदान करता है। धर्म के लिए कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं है। मोक्ष प्रदान करने में सहायक धर्म है। मनुष्य को जो अनाचारी और धर्मविरुद्ध बनाता है, वह अधर्म है। मनुष्य का ऊर्ध्वारोहण कर के ज्ञान और लक्ष्य की प्राप्ति धर्म कराता है। मनुष्य को आकृष्ट कर के सांसारिकता और अज्ञान के गम्भीर गर्त में अधर्म ही गिराता है।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।।८ ।।
शब्दार्थ : परित्राणाय-रक्षा के लिए, साधूनाम् सज्जनों की, विनाशाय-विनाश के लिए, च-और, दुष्कृताम् दुर्जनों के, धर्मसंस्थापनार्थाय-धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि -(मैं) जन्म लेता हूँ, युगे युगेयुग-युग में।
अनुवाद : सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट होता हूँ।
व्याख्या : साधूनाम् साधु वे हैं जो धर्म के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, शरीर से मानवता की सेवा करते हैं; स्वार्थ, काम और लोभ से परे हैं और परमात्मा के दिव्य ध्यान में भक्तिभाव से संलग्न रहते हैं।
दुष्कृताम् दुष्कृत् अथवा दुष्ट वे हैं जो अधर्म का जीवन यापन करते हैं, समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो व्यर्थ हैं, कुटिल हैं, लोभी हैं, हिंसापरायण हैं, बलात् दूसरों की सम्पत्ति पर अधिकार करते हैं और विभिन्न प्रकार के वीभत्स कुकृत्य करते हैं।
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ।।९।।
शब्दार्थ : जन्म-जन्म, कर्म-कर्म, च-और, मे-मेरे, दिव्यम् -दिव्य, एवम् इस प्रकार, यः-जो, वेत्ति-जानता है, तत्त्वतः - तत्त्व से (वास्तव में), त्यक्त्त्वा-त्याग कर, देहम्-शरीर को, पुनः-फिर, जन्म-जन्म, ननहीं, एति-प्राप्त करता है, माम् -मुझे, एति-प्राप्त करता है, सः- वह, अर्जुन-हे अर्जुन ।
अनुवाद : हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तथ्य रूप में जान लेता है, वह प्राण त्यागने के उपरान्त पुनः जन्म नहीं लेता, प्रत्युत् मुझे प्राप्त होता है।
व्याख्या : जन्म की अभिव्यक्ति का आभास होने पर भी भगवान् जन्म-मरण से परे हैं। प्रकट रूप में दृढ़तापूर्वक धर्म की संस्थापना में क्रियाशील होते हुए भी वे सब प्रकार के कर्म से परे हैं। इस सत्य को जान लेने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता । आत्मज्ञान प्राप्त कर के वह जीवन्मुक्त हो जाता है।
भगवान् का जन्म तो माया का एक खेल है। यह अप्राकृत है, दिव्य है, भगवान् की लीला है। मनुष्य रूप में दृष्टिगत होते हुए भी उनका शरीर चिन्मय होता है अर्थात् चेतन-स्वरूप होता है, पंचतत्त्वों से निर्मित मानव-शरीर की भाँति जड़ पदार्थ-सा नहीं होता।
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।।१०।।
शब्दार्थ : वीतरागभयक्रोधाः-अनुराग, भय और क्रोध से मुक्त, मन्मयाः- मुझ में अनुरक्त, माम्-मुझ में, उपाश्रिताः- आश्रित, बहवः बहुत, ज्ञानतपसा-ज्ञान रूपी अग्नि से, पूताः - परिमार्जित (पवित्र हुए), मद्भावम् -मेरे भाव को, आगताः-प्राप्त हुए।
अनुवाद : राग, भय और क्रोध से मुक्त हो कर, मुझमें लीन हो कर, मेरी शरण में आ कर, ज्ञान रूपी अग्नि में पवित्र हो कर अनेक भक्तों ने मेरे भाव को प्राप्त कर लिया है।
व्याख्या : आत्मज्ञान का सूर्य उदित होने पर ऐन्द्रिक विषयों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। यह ज्ञान होने पर कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नित्य, अविनाशी और शाश्वत आत्म-तत्त्व है तथा परिवर्तन मात्र शरीर का गुण है, वह (मनुष्य) अभय हो जाता है। सर्वथा आप्तकाम (इच्छाशून्य), स्वार्थ भाव से मुक्त और सर्वत्र आत्म-दर्शन करने वाला भला क्रोध का शिकार कैसे हो सकता है?
परब्रह्म में आश्रित पुरुष उसी ब्रह्म का भक्त हो जाता है। वह उसी में लीन हो जाता है अर्थात् ब्रह्मलीन अथवा ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है।
ज्ञानतपस्-ज्ञान की अग्नि । जिस प्रकार अग्नि रूई को जला देता है, उसी प्रकार ज्ञानतपस् समस्त सुप्त वृत्तियों, वासनाओं, तृष्णाओं, संस्कारों, पापों और समस्त कर्मों को जला कर साधकों को पवित्र कर देता है। (निरूपण - II.56; IV.19 से 37 तक)
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।११।।
शब्दार्थ : ये-जो, यथा-जिस प्रकार, माम् -मुझे, प्रपद्यन्ते-भजते हैं, तान् उनको, तथा उसी प्रकार से, एव-ही, भजामि भजता हूँ, अह्म - मैं, मम-मेरे, वर्म-मार्ग का, अनुवर्तन्ते-अनुसरण करते हैं, मनुष्याः मनुष्य, पार्थ-हे पार्थ, सर्वशः सब प्रकार से।
अनुवाद : हे अर्जुन, भक्तगण जिस प्रकार से भी मेरा भजन करते हैं, मैं उसी प्रकार से उन्हें भजता हूँ अर्थात् वैसा ही फल प्रदान करता हूँ। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं।
व्याख्या : जिस किसी भाव अथवा फल की आकाङ्क्षा से मनुष्य मेरा भजन करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन पर कृपा-दृष्टि करता हूँ। सकाम भाव से यदि कोई मुझे स्मरण करता है, तो उसको अभीष्ट पदार्थ प्रदान करता हूँ। यदि कोई ज्ञान की इच्छा से निष्काम भाव से मेरी आराधना करता है, तो उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। मैं किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता । (निरूपण—VII.21 और IX.23)
काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।।१२।।
शब्दार्थ : काङ्क्षन्तः इच्छा करते हुए, कर्मणाम् -कर्मों की, सिद्धिम् -सफलता, यजन्ते-यज्ञ करते हैं, इह-इस लोक में, देवताः- देवता, क्षिप्रम् - शीघ्र, हि-क्योंकि, मानुषे लोके-मनुष्य लोक में, सिद्धिः-सफलता, भवति होती है, कर्मजा-कर्म से उत्पन्न ।
अनुवाद : इस लोक में फल की इच्छा वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं; क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों का फल शीघ्र मिलता है।
व्याख्या : आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। इसके लिए पूर्ण त्याग आवश्यक है। साधक को पुरुषार्थ-चतुष्टय (अध्याय ३ का श्लोक ३ देखें) और अन्य अनेक गुणों से युक्त होने पर भी सतत घोर ध्यान का अभ्यास आवश्यक होता है; किन्तु सांसारिक (लौकिक) सिद्धि शीघ्र और सहज ही प्राप्त हो जाती है।
वर्णाश्रम और जाति पर आधारित वैदिक अनुष्ठान लौकिक मनुष्यों के लिए ही है।
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम् ।।१३ ।।
शब्दार्थ : चातुर्वर्ण्यम् - चार वर्ण, मया-मेरे द्वारा, सृष्टम्-बनाये गये हैं, गुणकर्मविभागशः गुण और कर्म के भेद से, तस्य-उसका, कर्तारम् -कर्ता, अपि-भी, माम् मुझको, विद्धि-जानो, अकर्तारम्-अकर्ता, अव्ययम् - अविनाशी, अपरिवर्तनशील ।
अनुवाद : गुण और कर्म के आधार पर मैंने चार वर्णों की रचना की। इस (वर्ण-व्यवस्था) का सृजनकर्ता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता ही जानो ।
व्याख्या : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-ये चार वर्ण गुण और कर्मों के अनुरूप बनाये गये हैं। ब्राह्मण में सत्त्व गुण की प्रधानता होती है। वह संयम, शुचिता, ऋजुता, सरलता, भक्ति आदि गुणों से सम्पन्न होता है। क्षत्रिय में रजोगुण की अधिकता होती है। वह पराक्रम, तेज, दृढ़ता, चातुर्य, उदारता और शासक स्वभाव से सम्पन्न होता है। वैश्य में रजोगुण मुख्य और तमोगुण गौण होता है। वह खेती-बाड़ी, पशुपालन और व्यापार आदि के अनुरूप गुणों से युक्त होता है। शूद्र में तमोगुण की प्रधानता रहती है और रजोगुण गौण रहता है। शूद्र अन्य तीन वर्णों की सेवा करता है। मानव-स्वभाव और वृत्ति गुणों की विभिन्नता से परिवर्तित होते हैं।
भगवान् कृष्ण वर्ण-व्यवस्था के सृष्टा होने पर भी अकर्ता होने से सृष्टा नहीं हैं। वे संसार में लिप्त नहीं हैं। वस्तुतः कर्तृत्वभाव तो माया वश है। माया ही सब-कुछ करती है। समाज में सुख-समृद्धि का राज्य हो, इसके लिए आवश्यक है कि चारों वर्ण अपना-अपना कर्म दक्षतापूर्वक करें, अन्यथा सर्वत्र लड़ाई-झगड़ा, कलह, भेद-भाव और संकीर्णता का साम्राज्य हो जाये। (निरूपण-XVIII.41)
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ।।१४ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, माम् -मुझे, कर्माणि-कर्म, लिम्पन्ति-लिप्त करते हैं, न-नहीं, मे—मेरी, कर्मफले-कर्मफल में, स्पृहा-लालसा, इति-इस प्रकार, माम् -मुझे, यः-जो, अभिजानाति-जानता है, कर्मभिः-कर्मों से, न-नहीं, सः वह, बध्यते-बँधता है।
अनुवाद : कर्म मुझे लिप्त नहीं करते और न ही मुझे किसी कर्मफल की कामना है। जो मुझे इस प्रकार से जान लेता है, वह बन्धन में नहीं आता।
व्याख्या : क्योंकि न तो मुझमें अहंभाव है और न ही कर्मफल की स्पृहा; अतः मैं कर्म के बन्धन में नहीं आता। सांसारिक लोग सोचते हैं कि वे तो प्रतिनिधि हैं और वे कर्म करते हैं। फिर कर्म के फल की भी कामना करते हैं। इसीलिए उन्हें पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। यदि वे अनासक्त हो कर अहंभाव और फल की आकाङ्क्षा का त्याग कर के कर्म करें, तो वे बन्धन में नहीं आयेंगे। वे जन्म-मरण से मुक्त हो जायेंगे। (निरूपण - IX.9)
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।
कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ।।१५ ।।
शब्दार्थ : एवम् - इस प्रकार, ज्ञात्वा-जान कर, कृतम् - किया गया, कर्म-कर्म, पूर्वैः- पूर्वजों द्वारा, अपि-भी, मुमुक्षुभि: -मोक्ष के जिज्ञासु साधकों द्वारा, कुरु-करो, कर्म-कर्म, एव-ही, तस्मात् - इसलिए, त्वम्-तुम, पूर्वैः- पूर्वजों द्वारा, पूर्वतरम् -पूर्वकाल में, कृतम् - किया गया।
अनुवाद : इस दिव्य ज्ञान को पा कर ही पुरातन काल में मुमुक्षु जनों ने कर्म किये; इसलिए तुम भी अपने पूर्वकाल के पूर्वजों की भाँति अनासक्त भाव से कर्म करो और अपने कर्तव्य का पालन करो।
व्याख्या : (हे अर्जुन), तुम इस सत्य को जान कर ही अपने कर्तव्य का पालन करो कि कर्मों के फल की स्पृहा आत्मा में नहीं हो सकती और न ही आत्मा इसमें लिप्त होती है और कोई भी व्यक्ति निष्काम भाव से अहंकार और आसक्तिशून्य हो कर कर्म करेगा, वह बन्धन में नहीं आयेगा।
यदि तुम्हारा हृदय अशुद्ध है, तो इसकी शुद्धि के लिए कर्म करो। यदि तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो संसार में पर-कल्याण हेतु कर्म करो। ऐसे ही कर्म प्राचीन काल में जनक आदि ने किये। अतः तुम भी कर्तव्य कर्म करो ।
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ।।१६ ।।
शब्दार्थ : किम् -क्या, कर्म-कर्म, किम् -क्या, अकर्म-अकर्म, इति-इस प्रकार, कवयः बुद्धिमान्, अपि-भी, अत्र-इसमें, मोहिताः- भ्रमित, तत्-वह, ते तुम्हें, कर्म-कर्म, प्रवक्ष्यामि बताऊँगा, यत्-जो, ज्ञात्वा-जान कर, मोक्ष्यसे- (तुम) मुक्त हो जाओगे, अशुभात्-दोषों से।
अनुवाद : कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में तो ज्ञानी जन भी भ्रमित हैं। मैं तुम्हें कर्म के विषय में ज्ञान दूँगा अर्थात् कर्म और अकर्म विषय को समझाऊँगा । कर्म की प्रकृति को जान कर तुम सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाओगे (संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाओगे) ।
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।।१७ ।।
शब्दार्थ : कर्मणः-कर्म का, हि-निश्चित रूप से, अपि -भी, बोद्धव्यम् बोध (ज्ञान) होना चाहिए, बोद्धव्यम्-बोध होना चाहिए, च-और, विकर्मणः - निषिद्ध कर्म का, अकर्मणः-अकर्म का, च-और, बोद्धव्यम् बोध होना चाहिए, गहना गहन, कर्मणः-कर्म की, गतिः गति ।
अनुवाद : निश्चित रूप से (शास्त्रविहित) कर्म की यथार्थ प्रकृति (रहस्य) का ज्ञान होना चाहिए। निषिद्ध कर्म और अकर्म का ज्ञान होना चाहिए। कर्म की गति को समझना अत्यन्त कठिन है (कर्मन् की गति न्यारी)।
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ।।१८ ।।
शब्दार्थ : कर्मणि-कर्म में, अकर्म - अकर्म, यः जो, पश्येत् देखे, अकर्मणि-अकर्म में, च-और, कर्म-कर्म, यः जो, सः वह, बुद्धिमान् बुद्धिमान्, मनुष्येषु मनुष्यों में, सः-वह, युक्तः योगी, कृत्स्नकर्मकृत् -सब कर्मों का कर्ता।
अनुवाद : कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखने वाला, मनुष्यों में ज्ञानी है। वह योगी है और सब कर्मों को करने वाला है।
व्याख्या : साधारण संभाषण की भाषा में हाथ-पैर और शरीर की गति (क्रिया) को कर्म कहा जाता है और शान्त हो कर निष्क्रिय बैठना अकर्म कहलाता है।
यह तो कारक का विचार है कि मैं कर्ता हूँ, जो मनुष्य को संसार के बन्धन में डालता है। यदि यह विचार न रहे, तो कर्म कर्म नहीं रह जाता। यह मनुष्य को बन्धन में नहीं डालेगा। यह कर्म में अकर्म है। यदि तुम प्रकृति की गतिविधियों को साक्षी भाव से देखो और यह अनुभव करो कि 'प्रकृति द्वारा ही सब कार्य हो रहे हैं, मैं तो अकर्ता हूँ', निष्काम आत्मा से (आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती) एकत्व स्थापित करो तो बस, कर्म चाहे कैसा और कितना ही क्यों न करो, तब कर्म कर्म नहीं होता। यह अकर्म है, कर्म में। इस प्रकार के अभ्यास से और भाव से कर्म अपनी बन्ध प्रकृति को त्याग देता है।
कोई मनुष्य शान्त बैठा रहे, निष्क्रिय बैठा रहे; किन्तु यदि उसमें कर्तापन का भाव रहता है, तो शान्त रहते हुए भी वह कर्म कर रहा है। यह अकर्म में कर्म है। चंचल मन सदा सक्रिय रहता है। यद्यपि मनुष्य चुपचाप बैठा हो, मन क्रियाशील है, तो कर्म हो रहा है। मन के कर्म ही वास्तविक कर्म हैं। क्षण-भर के लिए भी मनुष्य बिना कर्म किये नहीं रह सकता; क्योंकि प्रकृतिवश हो कर वह कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। (निरूपण – III.5)
अकर्म, अहंभाव को भी प्रेरित करता है। निष्क्रिय व्यक्ति कहता है-“मैं शान्त बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा", कर्म की भाँति अकर्म भी आत्मा पर मिथ्या रूप से आरोपित है।
इस सत्य को जानने वाला सब कर्मों का कर्ता है। उसने सब कर्मों का अन्त अर्थात् मोक्ष, ज्ञान अथवा पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया है।
जब एक अग्नि नौका (steamer) चलती है, तो तट पर लगे गतिहीन वृक्ष मानो विपरीत दिशा में चलते हुए दिखायी देते हैं। नौका में बैठे व्यक्ति को ऐसा आभास होता है। इसके विपरीत सुदूर दिशा में गतिशील पदार्थ जड़ अथवा गतिहीन से दृष्टिगोचर होते हैं। आत्मा के विषय में भी इसी भाँति कर्म को अकर्म में और अकर्म को कर्म में देखा जाता है।
आत्मा अकर्ता है, निष्क्रिय है। शरीर और इन्द्रियाँ कर्म करती हैं। अज्ञानी व्यक्ति शरीर और इन्द्रियों के कर्म को मिथ्या रूप से अकर्ता आत्मा में ही आरोपित करते हैं। इसीलिए अज्ञानी सोचता है-"मैं कर्ता हूँ।" वह आत्मा को कर्म का कर्ता अथवा प्रतिनिधि समझता है। यह भूल है, अज्ञान है।
जिस प्रकार से नौका में बैठे व्यक्ति को तट पर खड़े वृक्ष विपरीत दिशा में गति करते आभासित होते हैं, यद्यपि वे गतिहीन हैं, उसी प्रकार वस्तुतः कर्म आत्मा में नहीं होता।
आत्म-साक्षात्कार होने पर जन्म-मरण के कारक इस अज्ञान का विनाश हो जाता है।
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ।।१९ ।।
शब्दार्थ : यस्य-जिसके, सर्वे-समस्त, समारम्भाः-शास्त्रविहित कर्म, कामसंकल्पवर्जिताः- इच्छा और संकल्प से रहित, ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् - जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गये हैं तम् -उसे, आहु: -कहते हैं , पण्डितम् - ज्ञानी, बुधाः-विद्वान् ।
अनुवाद : जिसके समस्त कर्म कामनाशून्य और संकल्पशून्य हैं और जिसके कर्म ज्ञान रूप अग्नि में भस्म हो चुके हैं, ऐसे साधु पुरुष को विद्वान् लोग भी पण्डित कहते हैं।
व्याख्या : जनगण के समक्ष दृष्टान्त प्रस्तुत करने के भाव से ज्ञानी कर्म करता है। कर्म करते हुए भी वह कर्म नहीं करता; क्योंकि वह निःस्वार्थ है, क्योंकि आत्मज्ञान के द्वारा उसने कर्म में अकर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसके समस्त कर्म ज्ञानाग्नि में दग्ध हो चुके हैं। ब्रह्मज्ञान विशाल आध्यात्मिक अग्नि है जो शुभ-अशुभ सब प्रकार के कर्मफल का भक्षण करती है और तेजोद्दीप्त साधक को कर्म-बन्धन से मुक्त करता है। पूर्ण त्यागमय जीवन यापन करने वाला मुनि शरीर के निर्वाह के लिए अनिवार्य कर्म ही करता है। (निरूपण -III.19; IV.10, 37)
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किश्चित्करोति सः ।।२० ।।
शब्दार्थ : त्यक्त्वा-त्याग कर, कर्मफलासङ्गम् -कर्मफल के प्रति आसक्ति, नित्यतृप्तः - सदा सन्तुष्ट, निराश्रयः - आश्रय रहित, कर्मणि-कर्म में, अभिप्रवृत्तः - प्रवृत्त, अपि - भी, न-नहीं, एव-ही, किञ्चित् -कुछ भी, करोति-करता है, सः- वह ।
अनुवाद : कर्मफल के प्रति आसक्ति को त्याग कर, सर्वदा तृप्त रह कर और किसी का आश्रय न ले कर वह क्रियाशील होते हुए भी कुछ नहीं करता।
व्याख्या : साधक के मन में, कर्म में अकर्म के भाव को दृढ़ करने के लिए उसी तथ्य की पुनरावृत्ति की गयी है। वह जो विश्व में दूसरों के कल्याण में लगा है, फलासक्तिशून्य और अहंकारशून्य हो कर कर्म करता है, जनगण के समक्ष दृष्टान्त स्थापित करने के लिए कार्य करता है, वह सदा कर्म में रत रहते हुए भी वस्तुतः कुछ नहीं करता; क्योंकि वह आत्मज्ञानी है। उसने उस आत्मा से एकत्व स्थापित कर लिया जो कर्म से परे है।
क्योंकि ब्रह्मन्, परम पिता परमात्मा, स्वयंभू है, समस्त कामनाएँ स्वतः ही शान्त हो जाती हैं, जब उसका ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार से एक राजा का अनुग्रह प्राप्त होने पर किसी मनुष्य को किसी भी वस्तु के लिए मन्त्री अथवा सरकारी कार्यकर्ता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, उसी प्रकार परमात्मा पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति सर्वदा तृप्त रहता है, उसे किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता । (निरूपण-IV.41)
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ।।२१ ।।
शब्दार्थ : निराशीः- आशा रहित (आप्तकाम), यतचित्तात्मा-मन और बुद्धि को वश में करने वाला, त्यक्तसर्वपरिग्रहः-परिग्रह (स्वामित्व) का त्याग करने वाला, शारीरम् - शरीर के, केवलम् -केवल, कर्म-कर्म, कुर्वन् -करता हुआ, न-नहीं, आप्नोति -प्राप्त करता है, किल्बिषम् -पाप (दोष) को।
अनुवाद : किसी प्रकार की आकाङ्क्षा न रखते हुए, मन और बुद्धि को संयत कर के सब प्रकार के परिग्रह (लोभ लालच-स्वामित्व) का त्याग करने वाला व्यक्ति शरीर से कर्म करते हुए भी पाप का भागी नहीं बनता, उसे (कर्मफल का) दोष नहीं लगता।
व्याख्या : जीवन्मुक्त महापुरुष शरीर के निर्वाह के लिए अनिवार्य कर्म ही करता है, शेष समस्त कर्मों का त्याग कर देता है। वह समस्त भोग-सामग्री का भी त्याग कर देता है। अशुभ फल देने वाला वह कोई पाप कर्म नहीं करता । मुमुक्षु के लिए तो धर्म-कर्म भी पाप है; क्योंकि वह भी उसे संसार के बन्धन में डालेगा। धर्म एक स्वर्ण-पाश है। स्वर्ण-पाश भी तो पाश (बन्धन) ही है। ज्ञानी पुरुष धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ तथा पाप और पुण्य से मुक्त होता है। (निरूपण-III.7)
यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।। २२ ।।
शब्दार्थ : यदृच्छालाभसन्तुष्टः- स्वतः प्राप्त वस्तु से सन्तुष्ट, द्वन्द्वातीतः सुखदुःखादि द्वन्द्वों से परे, विमत्सरः- द्वेष रहित, समः समान, सिद्धौ-सफलता में, असिद्धौ-विफलता में, च-और, कृत्वा कर के, अपि-भी, न-नहीं, निबध्यते-बँधता ।
अनुवाद : जो मनुष्य स्वतःप्राप्त लाभ में सन्तुष्ट रहता है, जो द्वन्द्वों से परे है और ईर्ष्या रहित है, सिद्धि और असिद्धि अर्थात् सफलता और विफलता में सम (स्थिरधी) है, वह कर्म करते हुए भी उसके बन्धन में नहीं आता।
व्याख्या : स्वतःप्राप्त वस्तु में ज्ञानी पुरुष आनन्द में रहता है। चतुर्थ अध्याय के श्लोक १८ से २३ तक आत्म-ज्ञान के फल की पुनरुक्ति है, जो (ज्ञान) कर्म से अतीत है। 'कर्म रहित' आत्म-तत्त्व से एकत्व स्थापित करने वाला योगी बन्धन में नहीं आता; क्योंकि जन्म-मृत्यु के बन्धन में डालने वाले उनके कर्म और उसके कारण ब्रह्म-ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। आग में भस्म हो चुके बीज जिस प्रकार अंकुरित नहीं होते, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि में भस्म हुए कर्म भावी जन्म लाने में असमर्थ होते हैं।
सामान्य लोग एक ज्ञानी को कर्म करते देख कर उसे कर्ता, प्रतिनिधि, क्रियाशील और बन्धन में पड़ा हुआ मान लेते हैं। यह उनकी भूल है। अपनी ही दृष्टि में वह यथार्थतः प्रतिनिधि कदापि नहीं है। वह वास्तव में कोई कर्म नहीं करता। वह अनुभव करता है और कहता है- "मैं तो कुछ भी नहीं करता । प्रकृति करती है अथवा प्रकृति के तीन गुण ही सब-कुछ करते हैं।
वह सदा स्थिर रहता है; अतः शीत-उष्णता (सरदी-गरमी) सुख-दुःख, सफलता-विफलता उसे प्रभावित नहीं करते। शरीर के निर्वाह के लिए अनिवार्य सामग्री में भी उसकी आसक्ति नहीं रहती। शरीर के पोषण के लिए भोजन अथवा अन्य वस्तुएँ प्राप्त होने पर वह प्रसन्न नहीं होता और अप्राप्ति पर दुःखी नहीं होता। उसका कारण है कि वह अपनी मूल प्रकृति सत्-चित्-आनन्द (सच्चिदानन्द स्वरूप) में स्थित है। वह आनन्द के सागर में हिलोरें ले रहा है; इसीलिए वह शरीर और इसकी आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहता है।
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ।। २३ ।।
शब्दार्थ : गतसङ्गस्य-जिसकी आसक्ति समाप्त हो चुकी है, मुक्तस्य-मुक्त पुरुष का, ज्ञानावस्थितचेतसः- जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञाय-यज्ञ के लिए, आचरतः - आचरण करते हुए, कर्म-कर्म, समग्रम् -समस्त, प्रविलीयते-विलीन हो जाता है।
अनुवाद : उस व्यक्ति के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं जो यज्ञ (परमात्मा) के लिए कर्म करता है, आसक्ति रहित है, मुक्त है और जिसका चित्त ज्ञान में स्थित हो गया है।
व्याख्या : आसक्ति रहित, कर्म-बन्धन से मुक्त, ज्ञान में केन्द्रित चित्त वाले और केवल परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के सम्पूर्ण कर्म फल-सहित विलीन हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। वस्तुतः वे कर्म होते ही नहीं हैं।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।।२४ ।।
शब्दार्थ : ब्रह्म-ब्रह्म, अर्पणम्-आहुति, ब्रह्म-ब्रह्म, हविः- हवि (घृति), ब्रह्माग्नौ-ब्रह्म रूप अग्नि में, ब्रह्मणा-ब्रह्म के द्वारा, हुतम् - अर्पित किया गया, ब्रह्म-ब्रह्म, एव-ही, तेन-उसके द्वारा, गन्तव्यम् - प्राप्त किया जाता है, ब्रह्मकर्मसमाधिना-ब्रह्म रूपी कर्म में लीन व्यक्ति के द्वारा।
अनुवाद : ब्रह्म ही हव्य (आहुति) है, ब्रह्म ही घृत है, ब्रह्म रूप अग्नि में अर्पित किया जा रहा हव्य भी ब्रह्म है, वह सदा निश्चित रूप से ब्रह्म को ही प्राप्त होता है जो प्रत्येक कर्म में ब्रह्म को ही देखता है।
व्याख्या : यह ज्ञान-यज्ञ (wisdom-sacrifice) है जिसमें कर्म के साधन और सामग्री के भाव में ब्रह्मभाव का आदेश दिया गया है। इसमें कर्म भी ब्रह्म है और कर्म-फल भी ब्रह्म है। ऐसे भाव में प्रवेश पा लेने के पश्चात्, जैसा कि पूर्व-श्लोक (२३) में कहा है, सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं।
आत्म-साक्षात्कार होने पर सम्पूर्ण जीवन मानो एक ज्ञान-यज्ञ हो जाता है जिसमें हव्य सामग्री, घृत, यज्ञकर्ता, कर्म और लक्ष्य सभी ब्रह्म हैं। जो ब्रह्म पर इस विधि से पूर्ण ध्यान एकाग्रित करेगा, निश्चित रूप से ब्रह्म को प्राप्त होगा।
आत्म-ज्ञानी जानता है कि हव्य, अग्नि, उपकरण जिसके द्वारा घृत अग्नि में डाला जाता है और वह स्वयं, इन सबका ब्रह्म के अतिरिक्त स्व-अस्तित्व नहीं है। अपरोक्षानुभव में ब्रह्म का ज्ञान होने पर योगी कर्म करते हुए भी मानो कर्ता नहीं है। ज्ञानी के लिए सब कर्मों का अभाव ही हो जाता है। (निरूपण-III.15)
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ।। २५ ।।
शब्दार्थ : दैवम् -देवताओं से सम्बन्धित, एव-ही, अपरे अन्य, यज्ञम् यज्ञ, योगिनः-योगी, पर्युपासते-पूजा करते हैं, ब्रह्माग्नौ-ब्रह्म रूप अग्नि में, अपरे अन्य, यज्ञम्-यज्ञ, यज्ञेन-यज्ञ के द्वारा, एव-निश्चित रूप से, उपजुह्वति-अर्पित करते हैं।
अनुवाद : कुछ योगी जन देवाराधना रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, अन्य योगी, जिन्होंने आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा के द्वारा आत्मा को ही अर्पित कर दिया करते हैं।
व्याख्या : कर्मयोग में भक्तिभाव रखने वाले योगी देवताओं के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरा यज्ञ है 'ज्ञान-यज्ञ' (wisdom-sacrifice) जो ज्ञानियों द्वारा किया जाता है। इस यज्ञ में आहुति आत्मा की दी जाती है। यहाँ यज्ञ का अभिप्राय आत्मा से है। उपाधियाँ अथवा मर्यादित अनुबन्ध जैसे भौतिक शरीर, मन, बुद्धि आदि, जिनका ब्रह्म में अज्ञानवश अध्यारोपण किया जाता है, बोधातीत हो जाते हैं अर्थात् समाधि की अवस्था प्राप्त करने पर इन सबका बोध नहीं रह जाता और जीवात्मा परमात्मा से एकरूप हो जाता है। आत्मा को ब्रह्म में अर्पण करने का अभिप्राय है अपरोक्षानुभूति करना कि 'आत्मा ब्रह्म से पृथक् नहीं है, एक है।' यह सर्वोच्च ज्ञान है। ब्रह्मनिष्ठ योगी ऐसा ही यज्ञ करते हैं। अन्य सभी यज्ञों से यह यज्ञ उत्कृष्ट है।
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ।। २६ ।।
शब्दार्थ : श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि-श्रवणेन्द्रिय तथा अन्य इन्द्रियाँ, अन्ये-अन्य, संयमाग्निषु-संयम रूप अग्नि में, जुह्वति-हवन करते हैं, शब्दादीन् विषयान् - शब्दादि इन्द्रिय-विषय, अन्ये-अन्य, इन्द्रियाग्निषु-इन्द्रियों की अग्नि में, जुद्धति-यजन करते हैं।
अनुवाद : अन्य योगी जन संयम की अग्नि में श्रवणादि इन्द्रियों का हवन करते हैं, जब कि और योगी इन्द्रियों की अग्नि में शब्दादि विषयों का यजन करते हैं।
व्याख्या : कुछ योगी सतत इन्द्रिय-संयम में लगे रहते हैं। वे आत्मा के प्रकाश में इन्द्रियों को संहृत करके उन्हें उनके विषयों के सम्पर्क से रोकते हैं। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। अन्य योगी अपनी इन्द्रियों को पावन और अनिषिद्ध विषयों की ओर उन्मुख करते हैं। यह भी एक यज्ञ है।
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ।।२७ ।।
शब्दार्थ : सर्वाणि-सब, इन्द्रियकर्माणि-इन्द्रियों के कर्म, प्राणकर्माणि- प्राणों के कर्म, चऔर, अपरे—अन्य, आत्मसंयमयोगाग्नौ-आत्मसंयम रूप योग की अग्नि में, जुद्धति-आहुति देते हैं, ज्ञानदीपिते-जो ज्ञान द्वारा जलायी जाती है।
अनुवाद : अन्य साधक ज्ञान से उद्दीप्त आत्म-संयम की अग्नि में अन्य इन्द्रियों और प्राण की समस्त क्रियाओं को समर्पित करते हैं।
व्याख्या : जिस प्रकार तेल से दीप जलाया जाता है, उसी प्रकार आत्मसंयम की योगाग्नि ज्ञान से प्रज्वलित की जाती है। योगी जब अपने मन को आत्मा अथवा ब्रह्म पर एकाग्र करता है, तब इन्द्रियाँ और प्राण अपनी क्रिया त्याग कर शिथिल हो जाते हैं। इन्द्रियाँ और प्राण अपने कारण में विलीन हो जाते हैं।
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ।।२८ ।।
शब्दार्थ : द्रव्ययज्ञाः- वे लोग जो अपनी सम्पत्ति को यज्ञ में समर्पित करते हैं (सम्पत्ति का यज्ञ करने वाले लोग), तपोयज्ञाः- तपों का यज्ञ करने वाले, योगयज्ञाः योग का हवन करने वाले, तथा- इस प्रकार, अपरे अन्य, स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः स्वाध्याय और ज्ञान का यज्ञ करने वाले, च-और, यतयः यति (वानप्रस्थी) अथवा आत्म-संयत, संशितव्रताः-कठोर व्रतधारी ।
अनुवाद : अन्य अपनी भौतिक सम्पत्ति को, तपस्या को, योग को यज्ञ के रूप में समर्पित करते हैं, जब कि दृढ़ व्रतधारी और आत्म-संयमी मुनि जन अपने अध्ययन और ज्ञान का यजन करते हैं।
व्याख्या : दान के रूप में सुपात्र को सम्पत्ति दे कर कुछ लोग यज्ञ करते हैं। कुछ तपस्या में लीन हो जाते हैं, यही उनका यज्ञ है। अन्य कुछ अष्टाङ्गयोग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का समर्पण करते हैं। कुछ शास्त्राध्ययन करते हैं और इसे यज्ञ रूप में अर्पित करते हैं।
नोट : यम-पाँच महान् व्रत, नियम-सदाचार के पाँच नियम, आसन मुद्रा, प्राणायाम-श्वास पर नियन्त्रण, प्रत्याहार-इन्द्रियों को वश में करना, धारणा एकाग्रता, ध्यान-ध्यान, समाधि-तुर्यावस्था ।
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे ।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।।२९ ।।
शब्दार्थ : अपाने-अपान वायु में (निम्नगामी श्वास में), जुद्धति-अर्पित करते हैं, प्राणम् -प्राण को, प्राणे-भीतर आने वाले श्वास में, अपानम्-अपान को (बाह्य जाने वाले श्वास को), तथा- इस प्रकार, अपरे -अन्य, प्राणापानगती-बाहर और भीतर की वायु अर्थात् अपान और प्राण की गतियों को, रुद्ध्वा-रोक कर, प्राणायामपरायणाः केवल प्राणायाम में संलग्न अर्थात् श्वास-प्रश्वास पर संयम रखने का अभ्यास करने वाले ।
अनुवाद : अन्य योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और अन्य कोई प्राण में अपान का हवन करते हैं अर्थात् पूरक और रेचक प्राणायाम करते हैं। इस प्रकार श्वास-प्रश्वास की प्रक्रियाओं को रोक कर अन्य प्राणायाम-परायण योगी जन (कुम्भक द्वारा) श्वास को संयत करते हैं।
व्याख्या : कुछ योगी पूरक (श्वास भीतर खींचना) का अभ्यास करते हैं। अन्य रेचक (श्वास बाहर रोकना) का अभ्यास करते हैं और कुछ योगी कुम्भक (श्वास को रोकना) का अभ्यास करते हैं।
पाँच उप-प्राण एवम् अन्य प्राण, प्राणायाम के अभ्यास से मुख्य प्राण में लीन हो जाते हैं। प्राण का निग्रह होने पर मन भी इतस्ततः भागना त्याग कर स्थिर हो जाता है। इन्द्रियाँ भी सूक्ष्म हो कर प्राण में विलीन हो जाती हैं। प्राण के स्फुरण मात्र से मन और इन्द्रियों की प्रक्रियाओं को वश में रखा जाता है। प्राण संयत हो जाये, तो मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ अपना कार्य छोड़ देती हैं।
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।।३० ।।
शब्दार्थ : अपरे -अन्य लोग, नियताहाराः- आहार को नियमित करने वाले, प्राणान् -प्राणों को, प्राणेषु-प्राणों में, जुह्वति-अर्पित करते हैं, सर्वे-सब, अपि-भी, एते-ये, यज्ञविदः-यज्ञ के ज्ञाता, यज्ञक्षपितकल्मषाः - जिनके पाप यज्ञ से नष्ट हो चुके हैं।
अनुवाद : अन्य लोग अपना आहार नियमित कर के प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ये सब यज्ञ के ज्ञाता हैं जिनके समस्त पाप यज्ञ द्वारा नष्ट हो चुके हैं।
व्याख्या : 'नियताहाराः' का अभिप्राय है-नियमित अथवा अल्पाहार करने वाले । वे सन्तुलित भोजन करते हैं। आहार में कठोर नियमों का पालन कर के वे कर्मेन्द्रियों की प्रक्रियाओं को शिथिल कर के क्षुधा और वासना पर विजय प्राप्त करते हैं।
योगी अपनी प्राणवायु को वशीकृत (निग्रहीत) प्राण में डाल देते हैं। इस प्रकार प्राण मुख्य प्राण में विलीन हो जाता है।
उपर्युक्त यज्ञ के अनुष्ठान से मन परिमार्जित (शुद्ध) होता है और पापों का विनाश होता है।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।।३१ ।।
शब्दार्थ : यज्ञशिष्टामृतभुजः- यज्ञावशेष रूप अमृत का पान करने वाले, यान्ति-प्राप्त होते हैं, ब्रह्म-ब्रह्म को, सनातनम् -सनातन, न-नहीं, अयम् यह, लोकः-लोक, अस्ति- है, अयज्ञस्य-यज्ञ न करने वाले का, कुतः कहाँ से, अन्यः-अन्य, कुरुसत्तम-कुरुश्रेष्ठ ।
अनुवाद : हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अमृत समान यज्ञावशेष का सेवन करने वाले शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले के लिए तो यह संसार ही (सुखद) नहीं है, फिर परलोक की तो बात ही क्या?
व्याख्या : ऊपर वर्णित शास्त्रविहित यज्ञों का अनुष्ठान कर के मन शुद्ध होने पर आत्म-ज्ञान प्राप्त कर के समय के साथ योगी जन सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उनमें से किसी भी यज्ञ का पालन न करने वाला इस दुःखमय लोक के लिए भी उपयुक्त नहीं है, फिर इससे श्रेष्ठतर लोक की वह कामना भी कैसे कर सकता है? (निरूपण-III.13)
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।।३२ ।।
शब्दार्थ : एवम् - इस प्रकार, बहुविधाः- अनेक प्रकार के, यज्ञाः यज्ञ, वितताः - विस्तीर्ण हैं (बताये गये हैं), ब्रह्मणः - ब्रह्म अथवा वेद के, मुखे-मुख में, कर्मजान् -कर्म से उत्पन्न, विद्धि-जानो, तान्-उन, सर्वान् -सबको, एवम् - इस प्रकार, ज्ञात्वा-जान कर, विमोक्ष्यसे मुक्त हो जाओगे।
अनुवाद : इस प्रकार वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। उन्हें कर्म से उत्पन्न हुआ जानो । ऐसे ज्ञान प्राप्त कर के तुम बन्धन-मुक्त हो जाओगे ।
व्याख्या : 'ब्रह्मणः' का अर्थ वेदों में ऐसा भी निरूपित किया गया है।
अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख में विस्तृत हैं अर्थात् वेदों में आचक्षित हैं। उन्हें कर्म से उत्पन्न हुआ ही जानो; क्योंकि आत्मा कर्म से परे है। यदि तुम्हें यह ज्ञान हो जाये कि इन कर्मों का तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं, वे कर्म तुम्हारे नहीं हैं और तुम कर्म रहित (निष्काम) हो, तो इस सम्यक् ज्ञान को प्राप्त कर निश्चित रूप से तुम संसार के बन्धन से मुक्त हो जाओगे। (निरूपण - IX.27; XIII.15)
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।। ३३ ।।
शब्दार्थ : श्रेयान् - अधिक अच्छा, द्रव्यमयात् द्रव्यमय (से), यज्ञात् यज्ञ से, ज्ञानयज्ञः- ज्ञान-यज्ञ, परन्तप - हे शत्रुओं को सताने वाले, सर्वम् सर्व, कर्म-कर्म, अखिलम् -पूर्ण रूप से, पार्थ-अर्जुन, ज्ञाने-ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त होते हैं।
अनुवाद : हे अर्जुन, द्रव्य (सामग्री) द्वारा किये जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ अधिक अच्छा है; क्योंकि अन्ततोगत्वा सब कर्म पूर्णतया ज्ञान में ही समाप्त होते हैं।
व्याख्या : भौतिक पदार्थों से किये जाने वाले यज्ञ भौतिक कार्यों (effects) के कारण (cause) बनते हैं और उसका फल भोगने के लिए यज्ञकर्ता को इस भौतिक जगत् में पुनः अवतरित होना पड़ता है। ज्ञान-यज्ञ मोक्षप्रद होता है। जैसे नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त कर्मों का अन्तर्भाव ज्ञान में होता है। समस्त कर्म हृदय को परिमार्जित करते हुए ज्ञानोदय की ओर अग्रसर करते हैं। आत्म-ज्ञान में ही कर्मों का अन्त है।
परमात्मा को समर्पित किये गये फल सहित सारे कर्म ब्रह्मज्ञान में निहित हैं। (निरूपण-IX.15; X.25; XVIII.70)
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।। ३४ ।।
शब्दार्थ : तत् -वह, विद्धि-जानो, प्रणिपातेन-दण्डवत् प्रणाम द्वारा, परिप्रश्नेन-प्रश्न द्वारा, सेवया-सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति-उपदेश देंगे, ते-तुम्हें, ज्ञानम् ज्ञान, ज्ञानिनः- ज्ञानी जन, तत्त्वदर्शिनः सत्य को जानने वाले ।
अनुवाद : उस ज्ञान का उपदेश तुम्हें तत्त्वदर्शी (ज्ञानी) लोग देंगे। उसे तुम दण्डवत् प्रणाम द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और सेवा से प्राप्त करो।
व्याख्या : शास्त्रों में पारंगत ब्रह्मश्रोत्रिय अथवा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाओ। पूर्ण भक्तिभाव से सविनय दण्डवत् प्रणाम करो। प्रश्न पूछो-"हे समादरणीय गुरुदेव ! बन्धन का कारण क्या है? मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ? अज्ञान की प्रकृति क्या है? ज्ञान की प्रकृति क्या है? आत्म-साक्षात्कार हेतु अन्तरङ्ग साधना क्या है?" श्रद्धाभाव से गुरु की सेवा करो। शास्त्र में निपुण होने पर भी आत्म-ज्ञानी न होने पर गुरु तुम्हें आत्म-ज्ञान नहीं दे सकता। उस ज्ञान को प्राप्त करने अथवा ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए तुम्हें ऐसे गुरु के पास ही जाना होगा जो शास्त्र-निपुण भी हो और ब्रह्मज्ञानी भी हो। मात्र प्रणिपात से ज्ञान नहीं मिलेगा। उसमें दम्भ का आभास हो सकता है। गुरु में अपूर्व श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए । श्रद्धा और भक्तिभाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए, तब दम्भ के लिए स्थान नहीं रहेगा।
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ।।३५ ।।
शब्दार्थ : यत्-जो, ज्ञात्वा-जान कर, न -नहीं, पुनः -पुनः, मोहम् -मोह को, एवम् - इस प्रकार, यास्यसि-प्राप्त करोगे, पाण्डव- हे पाण्डव, येन-जिसके द्वारा, भूतानि-प्राणी, अशेषेण-सभी, द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि-(निज) आत्मा में, अथो-भी, मयि - मुझमें।
अनुवाद : हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करने पर तुम पुनः भ्रम में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान से तुम समस्त प्राणियों को अपने भीतर और फिर मुझमें भी देखोगे ।
व्याख्या: पूर्व श्लोक में निर्दिष्ट आत्म-ज्ञान, जो प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा द्वारा ब्रह्मनिष्ठ गुरु से प्राप्त करना है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर तुम पुनः भ्रमित नहीं होओगे। तुम तो उस मूल एकत्व का दर्शन करोगे। अपरोक्षानुभूति में, अथवा अपनी आत्मा के आलोक में अथवा भावातीत ज्ञान में तुम अनुभव करोगे कि सृष्टिकर्ता से ले कर तृण पर्यन्त समस्त प्राणी तुम्हारे भीतर हैं और मुझमें भी हैं। (निरूपण - IX.15; XVIII.20)
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ।। ३६ ।।
शब्दार्थ : अपि-भी, चेत्-यदि, असि-हो, पापेभ्यः -पापियों से, सर्वेभ्यः सभी (से), पापकृत्तमः-सर्वाधिक पापी, सर्वम् -सब, ज्ञानप्लवेन-ज्ञान रूपी नौका से, एव-ही, वृजिनम् -पाप, सन्तरिष्यसि-पार कर जाओगे।
अनुवाद : यदि तुम अन्य पापियों से भी अपेक्षाकृत अधिक पापी हो, तो भी निश्चित रूप से ज्ञान रूपी नौका द्वारा पाप के सागर से तर जाओगे।
व्याख्या : तुम आत्म-ज्ञान की नाव से पाप के सागर के पार पहुँच सकते हो। (निरूपण-IX.30)
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुते ऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।। ३७ ।।
शब्दार्थ : यथा-जैसे, एधांसि-ईंधन को, समिद्धः जलती हुई, अग्निः-अग्नि, भस्मसात्कुरुते-भस्म कर देता है, अर्जुन-हे अर्जुन, ज्ञानाग्निः- ज्ञान रूपी अग्नि, सर्वकर्माणि-सब कर्मों को, भस्मसात्कुरुते-भस्म कर देता है, तथा-वैसे ही।
अनुवाद : हे अर्जुन, जिस प्रकार से प्रज्ज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है।
व्याख्या : जले हुए बीज जिस प्रकार अंकुरित नहीं हो सकते, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि में दग्ध कर्म भी फल नहीं दे सकते अर्थात् कर्म-फल को भोगने के लिए तब मनुष्य को इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ेगा। कर्म को भस्मसात् करना यही है। ज्ञानाग्नि में दग्ध हो कर कर्म अपनी शक्ति खो देते हैं। ज्ञानोदय होने पर अग्नि में ईंधन की भाँति ज्ञान में कर्म भस्म हो जाते हैं। जब अहंभाव शून्य को प्राप्त हो गया, कामनाएँ नहीं रहीं, फल की इच्छा शून्य हो गयी तो कर्म नहीं रहा । इसकी शक्ति समाप्त हो गयी। जिन प्रारब्ध कर्मों के कारण यह शरीर सत्ता में आया है और प्रारब्ध कर्म का फल भोग रहा है, उन प्रारब्ध कर्मों को छोड़ कर अन्य सभी कर्मों को ज्ञानाग्नि भस्म करने में समर्थ है। शंकराचार्य अपनी अपरोक्षानुभूति में तो प्रारब्ध कर्मों के भी भस्म होने की बात लिखते हैं।
वेद में भी स्पष्ट रूप से कर्मों के नष्ट होने का तथ्य बहुवचन में वर्णित है-"उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है", स्वाभाविक है, यहाँ प्रारब्ध कर्म से भी वेद का तात्पर्य रहा है।
पूर्वकृत् कर्मों के फल, प्रतिक्रिया अथवा कर्म तीन प्रकार के हैं। प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जिनके कारण यह शरीर मिला है। संचित कर्म वे अवशिष्ट कर्म हैं जो भावी जन्म प्रदान करेंगे, वे हमारे ही द्वारा संचित किये गये हैं। आगामी अथवा क्रियमाण वे कर्म हैं जो इस जन्म में हम कर रहे हैं। यदि दिव्य आत्म-ज्ञान से संचित और क्रियमाण कर्म ही नष्ट होने की बात होती तो द्विवचन का प्रयोग होता, बहुवचन का नहीं (संस्कृत व्याकरण में वचन तीन हैं-एक वचन, द्विवचन और बहुवचन) । (निरूपण - IV. 10-19)
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।। ३८ ।।
शब्दार्थ : न -नहीं, हि-निस्सन्देह, ज्ञानेन-ज्ञान की अपेक्षा, सदृशम् -समान, पवित्रम् - पवित्र, इह-यहाँ (इस लोक में), विद्यते-है, तत्-वह, स्वयम् स्वयम्, योगसंसिद्धः- योग में पारंगत (योगी), कालेन समय के साथ, आत्मनि-आत्मा में, विन्दति-प्राप्त करता है।
अनुवाद : निःसन्देह, ज्ञान सदृश पवित्र करने वाली इस संसार में दूसरी वस्तु नहीं है। योग में पारंगत होने पर मनुष्य स्वयं ही उस ज्ञान को समय आने पर अपने भीतर प्राप्त कर लेता है।
व्याख्या : आत्म-ज्ञान के समान पवित्र करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। कर्मयोग और ध्यानयोग में पूर्णत्व प्राप्त कर लेने पर मनुष्य समय के साथ स्वयं ही उस आत्म-ज्ञान की अनुभूति करता है।
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।। ३९ ।।
शब्दार्थ : श्रद्धावान्-श्रद्धायुक्त, लभते - प्राप्त करता है, ज्ञानम् - ज्ञान को, तत्परः-तत्पर, संयतेन्द्रियः - इन्द्रियों को वश में करने वाला, ज्ञानम्-ज्ञान, लब्ध्वा-प्राप्त करके, पराम् -परम, शान्तिम् - शान्ति को, अचिरेण-शीघ्र ही, अधिगच्छति -प्राप्त करता है।
अनुवाद : ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो विजितेन्द्रिय है अर्थात् जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, जो तत्पर (भक्तिभाव से पूर्ण है) है और श्रद्धा युक्त है। ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वह शीघ्र ही परम शान्ति को प्राप्त करता है।
व्याख्या : श्रद्धा-विश्वास से युक्त व्यक्ति जो सतत गुरु की सेवा में संलग्न है और उनके उपदेशों का श्रवण करता है तथा जिसने अपनी इन्द्रियों को वशीभूत कर लिया है, वह निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करता है और परम शान्ति की अथवा मोक्ष की अनुभूति करता है। अचिरेण परम शान्ति प्राप्त्यर्थ ऊपर वर्णित तीनों गुणों की महत्वाकांक्षा अनिवार्य है। मात्र एक ही गुण पर्याप्त नहीं है। (निरूपण-X.10,11)
अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुख्खं संशयात्मनः ।।४० ।।
शब्दार्थ : अज्ञः- अज्ञानी, च-और, अश्रद्दधानः-श्रद्धा रहित, च-और, संशयात्मा-संशय युक्त, विनश्यति - नष्ट हो जाता है, न-नहीं, अयम्-यह, लोकः लोक, अस्ति-है, न-नहीं, परः-परलोक, न-नहीं, सुख्खम् -सुख, संशयात्मनः-संशयालु का।
अनुवाद : अज्ञानी (विवेक रहित), श्रद्धा रहित, संशय युक्त व्यक्ति तो विनाश को ही प्राप्त होता है। संशय करने वाले के लिए तो न यह लोक है, न परलोक है और न कहीं सुख ही है।
व्याख्या : आत्म-ज्ञान से शून्य व्यक्ति अज्ञानी है, श्रद्धारहित वह है जिसे न तो अपनी आत्मा में विश्वास है, न शास्त्रों में, न ही गुरु के उपदेशों में विश्वास है।
संशय युक्त व्यक्ति संसार में सर्वाधिक पापी है। उसकी दशा तो शोचनीय है। परलोक के विषय में भी वह तो शंका से पूर्ण है। संशय-बुद्धि होने के कारण वह इस लोक में प्रमुदित नहीं हो सकता। वह सुखी नहीं है।
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।।४१ ।।
शब्दार्थ : योगसंन्यस्तकर्माणम् - जिसने योग की विधि से सारे कर्मों का त्याग कर दिया है, ज्ञानसंछिन्नसंशयम् - विवेक द्वारा जिसके संशय नष्ट हो चुके हैं, आत्मवन्तम् - आत्म-परायण, न-नहीं, कर्माणि-कर्म, निबध्नन्ति-बाँधते हैं, धनञ्जय-हे धनञ्जय ।
अनुवाद : हे धनञ्जय (अर्जुन), जिसने योग-विधि से कर्मों से संन्यास ले लिया है, (आत्म) ज्ञान से जिसके संशय समाप्त हो गये हैं और जो आत्म-परायण हो गया है, उसे कर्म-बन्धन नहीं होता।
व्याख्या : मधुसूदन सरस्वती 'आत्मवन्तम्' का अर्थ 'सदा जागरूक' (always watchful) करते हैं।
आत्म-ज्ञानी योग-विधि से कर्मों का त्याग करता है अर्थात् समस्त कर्म परमात्मा को समर्पित कर के करता है। आत्म-तत्त्व का परमात्म-तत्त्व में एक होने का अनुभव प्राप्त कर लेने पर उसके समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं। अब कर्म उसे बाँधते नहीं; क्योंकि वे ज्ञानाग्नि में दग्ध हो चुके हैं और अब वह सदा आत्म-जागृति में आनन्द लेता है। (निरूपण - II.48; III.9; IV.20)
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनाऽऽत्मनः ।
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।।४२ ।।
शब्दार्थ : तस्मात् - इसलिए, अज्ञानसंभूतम् - अज्ञान से उत्पन्न, हत्स्थम् -हृदय में निहित, ज्ञानासिना- ज्ञान की तलवार से, आत्मनः- आत्मा का, छित्त्वा काट कर, एनम्-इस, संशयम्सन्देह, योगम् - योग का, आतिष्ठ-शरण लो, उत्तिष्ठ-उठो, भारत- हे अर्जुन।
अनुवाद : इसलिए हे अर्जुन, उठो, योग की शरण लो और अज्ञानवश हृदय में उत्पन्न सन्देह को आत्म-ज्ञान की तलवार से छिन्न-भिन्न कर दो।
व्याख्या : संशय मानसिक पीड़ा को जन्म देता है। यह अत्यन्त पापी है। यह अज्ञान से उत्पन्न है। इसे ज्ञान रूपी खड्ग से निर्दयतापूर्वक मार डालो । हे अर्जुन, अब उठो और युद्ध करो।
(यह अध्याय ज्ञानयोग, अभ्यासयोग अथवा ज्ञानकर्मसंन्यासयोग से भी अभिहित है।)
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
ज्ञानविभागयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ।।
।। इति ज्ञानविभागयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ पञ्चमोऽध्यायः
कर्मसंन्यासयोगः
अर्जुन उवाच
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ।।१ ।।
शब्दार्थ : संन्यासम् -संन्यास, कर्मणाम् -कर्मों का, कृष्ण-हे कृष्ण, पुनः पुनः, योगम् योग, च-और, शंससि–प्रशंसा करते हो, यत्-जो, श्रेयः-कल्याणकारी, एतयो:- इन दोनों में, एकम् -एक, तत्-वह, मे-मुझे, ब्रूहि-बतायें, सुनिश्चितम् - निश्चित रूपेण ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं और पुनः योग की प्रशंसा करते हैं। मुझे निश्चित रूप से बताएँ, इन दोनों में अधिक श्रेयस्कर क्या है।
व्याख्या : आप कर्मों के संन्यास का और फिर उनके अनुष्ठान का उपदेश करते हैं। इससे मैं भ्रमित हो रहा हूँ। दोनों में से जो अधिक श्रेयस्कर हो, वह मार्ग मुझे प्रशस्त करें। एक ही समय में दोनों का आश्रय लेना मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है। योग का अभिप्राय यहाँ कर्मयोग से है। (निरूपण - III.2)
श्री भगवानुवाच
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।।२।।
शब्दार्थ : संन्यासः-संन्यास, कर्मयोग:-कर्म का योग, च-और, निःश्रेयसकरौ- परम आनन्द की ओर ले जाने वाले, उभौ-दोनों, तयो:-उन दोनों में से, तु-लेकिन, कर्मसंन्यासात् -कर्म-त्याग से, कर्मयोगः कर्मयोग, विशिष्यते -अधिक अच्छा है।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम आनन्द की प्राप्ति कराने वाले हैं, पुनरपि, कर्म-संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अधिक कल्याणप्रद है।
व्याख्या : संन्यास (कर्म का त्याग) अथवा कर्मयोग (कर्मानुष्ठान) दोनों ही मोक्षप्रद हैं, आनन्ददायी हैं। यद्यपि दोनों मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, तथापि मोक्ष-प्राप्ति के दो साधनों में से आत्मज्ञान-शून्य, कर्मसंन्यास की अपेक्षा (निष्काम भाव से) कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। इसमें विवेक-बुद्धि से कर्म का संन्यास निःसन्देह कर्मयोग से श्रेष्ठ है। कर्मयोग सरल है; अतः सभी के लिए अपेक्षित है। (निरूपण-III.3; V.5; VI.46)
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ।।३ ।।
शब्दार्थ : ज्ञेयः -जाना जाये, सः- वह, नित्यसंन्यासी-सदा संन्यासी, यः जो, न नहीं, द्वेष्टि-द्वेष करता है, न-नहीं, काङ्क्षति-इच्छा करता है, निर्द्वन्द्वः - द्वन्द्वों से मुक्त, हि-निस्सन्देह, महाबाहो - हे महाबाहो (अर्जुन), सुखम् - सहज ही, बन्धात् बन्धन से, प्रमुच्यते-मुक्त हो जाता है।
अनुवाद : हे अर्जुन, जो मनुष्य समस्त द्वन्द्वों से परे है, न किसी से द्वेष करता है, न कोई कामना करता है और जिसमें सदा त्याग की भावना विद्यमान रहती है, ऐसा मनुष्य सदा संन्यासी ही समझा जाना चाहिए। वह सहज ही सब प्रकार के बन्धन से मुक्त हो जाता है।
व्याख्या : व्यवसाय न होने पर, विपत्ति आने पर, परिवार की कलह के कारण, अज्ञानवश अथवा आलस्यवश कर्म का त्याग करने वाला व्यक्ति संन्यासी नहीं होता। एक सच्चा संन्यासी दम्भी और कायर नहीं होता ।
कर्मरत रहने पर भी वह नित्यसंन्यासी है, कर्मयोगी है जो दुःख से घृणा नहीं करता और दुःख देने वाले विषयों के प्रति भी उदार रहता है, न ही उसे सुख की अथवा सुख देने वाले पदार्थों की कामना होती है। किसी भी इन्द्रिय-विषय के प्रति उसमें न तो आसक्ति रहती है और न ही अनासक्ति । वह शीत-ग्रीष्म, दुःख-सुख, असफलता-सफलता, जय-पराजय, हानि-लाभ, मान-अपमान, यश-अपयश के द्वन्द्वों से अतीत रहता है।
किसी ने विधिवत् संन्यास न लिया हो, किन्तु उसमें ऊपर वर्णित मानसिक भावनाएँ हैं तो वह सदा संन्यासी ही माना जायेगा। आवश्यकता है तो बस कामना रहित, अहंकार शून्य शुद्ध हृदय की । भौतिक पदार्थों का त्याग संन्यास नहीं है। (निरूपण –VI.1)
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ।।४।।
शब्दार्थ : सांख्ययोगौ-सांख्य (ज्ञान) और योग (कर्मयोग), पृथक् -भिन्न, बालाः बालक (अल्पज्ञ), प्रवदन्ति-कहते हैं, न-नहीं, पण्डिताः - विद्वान्, एकम् -एक, अपि-भी, आस्थितः - स्थित, सम्यक् -पूर्णतया, उभयोः दोनों का, विन्दते-प्राप्त करता है, फलम् -फल ।
अनुवाद : ज्ञानयोग (सांख्य) और कर्मयोग (योग) को अल्पज्ञ ही पृथक् मानते हैं, पण्डित (ज्ञानी) नहीं। इन दोनों में से एक में भी पूर्णतः स्थित होने पर व्यक्ति दोनों का फल प्राप्त करता है।
व्याख्या : बालाः- अज्ञानी लोग, जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान तो है; परन्तु वे आत्म-ज्ञान से वंचित हैं। अल्पज्ञ ही ऐसा सोचते हैं कि सांख्य और योग का पृथक् प्रभाव होता है और दोनों पृथक् परिणाम के देने वाले हैं। किन्तु बुद्धिमान् लोगों का कथन है कि ये दोनों एक ही परिणाम-मोक्ष को देने वाले हैं। दोनों में से एक में भी जो भलीभाँति स्थित है अर्थात् जो सांख्ययोग अथवा कर्मयोग में पूर्णतः निष्ठावान् है, वह दोनों का फल प्राप्त करता है। अतः फल में विभिन्नता नहीं है, यही इस श्लोक का सार-तत्त्व है। (निरूपण - V1.2)
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।।५ ।।
शब्दार्थ : यत्-जो, सांख्यैः-सांख्य के द्वारा, प्राप्यते-प्राप्त किया जाता है, स्थानम् -स्थान, तत्-वह, योगैः- योगियों के द्वारा, अपि -भी, गम्यते-पहुँचा जाता है, एकम् - एक, सांख्यम् -सांख्य (ज्ञान), च-और, योगम् योग, चऔर, यः- जो, पश्यति - देखता है, सः वह, पश्यति-वास्तव में देखता है।
अनुवाद : सांख्य अथवा ज्ञानयोगी जिस धाम को पहुँचते हैं कर्मयोगी भी उसी धाम को प्राप्त करते हैं। जो सांख्ययोग और कर्मयोग को समान रूप से देखता है, वही वस्तुतः देखता है।
व्याख्या : संसार को त्याग कर जो ज्ञानयोग अथवा वेदान्त-मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे सांख्ययोगी हैं। श्रवण (श्रुति अथवा उपनिषद् शास्त्रों को सुनना), मनन (श्रवण किये हुए का चिन्तन) और निदिध्यासन (सतत गहन ध्यान) द्वारा वे मोक्ष अथवा कैवल्य की प्राप्ति करते हैं अर्थात् अपरोक्षानुभूति करते हैं। निष्काम सेवा करने वाले कर्मयोगी, जो फल की इच्छा त्याग कर भक्तिभाव से कर्म करते हुए भगवान् को सब कर्म समर्पित कर देते हैं, वे हृदय-शुद्धि, त्याग और परिणाम स्वरूप आत्मज्ञानोदय से सांख्ययोगियों की भाँति अपरोक्षानुभूति से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। सांख्य और योग दोनों को सम रूप से देखने वाला ही वास्तव में देखता है। (निरूपण—XIII.24, 25; V.2)
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ।।६ ।।
शब्दार्थ : संन्यासः-त्याग, तु-लेकिन, महाबाहो - हे महाबाहो (अर्जुन), दुःखम् - दुःख, आमुम् - पाने के लिए, अयोगतः - बिना योग के, योगयुक्तः- योग में समन्वित, मुनिः-मुनि, यति, ब्रह्म-ब्रह्म को, नचिरेण-शीघ्र ही, अधिगच्छति - प्राप्त करता है।
अनुवाद : किन्तु हे अर्जुन, बिना योग के संन्यास ग्रहण करना दुष्कर है। योग में निष्ठावान् यति ही शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त होता है।
व्याख्या : मुनि वह है जो मनन (ध्यान, आत्म-विश्लेषण) करता है। योग, निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित किया गया कर्म है।
ब्रह्म शब्द यहाँ संन्यास को संकेत करता है; क्योंकि आत्म-ज्ञान में ही संन्यास (त्याग) निहित है। कर्मयोग से परिष्कृत यति, मुनि, ध्यान योगी और योग में समन्वित पुरुष अविलम्ब ब्रह्म प्राप्ति करता है। यही सच्चा संन्यास है और यही आत्म ज्ञान के प्रति भक्ति है। अतः कर्मयोग श्रेष्ठतर है। नव साधक के लिए यह सुगम है। मन की शुद्धि के द्वारा कर्मयोग साधक को उच्चतर योग के लिए प्रेरित करता है।
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ।।७ ।।
शब्दार्थ : योगयुक्तः कर्मयोग के प्रति निष्ठावान्, विशुद्धात्मा - पवित्र मन वाला, विजितात्मा-आत्मा का स्वामी, जितेन्द्रियः - इन्द्रियों पर विजय पाने वाला, सर्वभूतात्मभूतात्मा-अपनी आत्मा को सब प्राणियों की आत्मा में देखने वाला, कुर्वन् -करते हुए, अपि-भी, न-नहीं, लिप्यते-लिप्त होता ।
अनुवाद : जो कर्मयोग में रत है, जिसका अन्तःकरण विशुद्ध है, जो जितेन्द्रिय और आत्मा का स्वामी है तथा जो सर्वभूतों में निज आत्मा के दर्शन करता है, वह योगी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता।
व्याख्या : जो योगयुक्त है अर्थात् जिसने कर्मयोग के द्वारा अपना अन्तःकरण विशुद्ध कर लिया है, जिसने अपने शरीर और इन्द्रियों को वश में कर लिया है, जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा है, वह पुरुष परोपकार हेतु अथवा जनगण के समक्ष दृष्टान्त रखने हेतु कर्म करते हुए भी कर्म में आसक्त नहीं होता। (निरूपण-XVIII.17)
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
पश्यन् शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्ननाच्छन्स्वपन् श्वसन् ।।८ ।।
शब्दार्थ : न -नहीं, एव-ही, किंचित्-कुछ भी, करोमि - करता हूँ, इति-इस प्रकार, युक्तः- आत्म-केन्द्रित, मन्येत-सोचे, तत्त्ववित्-सत्य का ज्ञाता, पश्यन् देखता हुआ, शृण्वन् -सुनता हुआ, स्पृशन् -स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् -सूँघता हुआ, अश्नन् - खाता हुआ, गच्छन् - जाता हुआ, स्वपन् सोता हुआ, श्वसन् श्वास लेता हुआ।
अनुवाद : "मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा चिन्तन एक तत्त्वज्ञानी का होता है-दर्शन करते हुए, श्रवण करते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, गमन करते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए,
प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ।।९ ।।
शब्दार्थ : प्रलपन् बात करते हुए, विसृजन् - त्याग करते हुए, गृह्वन् - ग्रहण करते हुए, उन्मिषन् -पलक झपकते हुए, निमिषन् बन्द करते हुए, अपि-भी, इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ, इन्द्रियार्थेषु -इन्द्रिय-विषयोंमें, वर्तन्ते-बरतते हैं, इति-इस प्रकार, धारयन् - धारण करते हुए।
अनुवाद : बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, नेत्र बन्द करते और खोलते हुए वह मान लेता है कि मात्र इन्द्रियों के विषयों में इन्द्रियाँ क्रियाशील हैं।
व्याख्या : एक मुक्तात्मा इन्द्रियों की प्रक्रियाओं का सदा साक्षी बन कर रहता है; क्योंकि उसने ब्रह्मैक्य प्राप्त कर लिया है। वह सोचता है और कहता है- 'मैं नहीं देखता, नेत्र देखते हैं; मैं नहीं सुनता, कर्ण सुनते हैं; मैं नहीं सूँघता, नासिका सूँघती है' इत्यादि। वह कर्म में अकर्म देखता है; क्योंकि ज्ञान की अग्नि ने उसके समस्त कर्म दग्ध कर दिये हैं। (निरूपण - XIV. 19-23)
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।१०।।
शब्दार्थ : ब्रह्मणि-ब्रह्म में, आधाय-समर्पित कर के, कर्माणि-कर्म, सङ्गम् - आसक्ति, त्यक्त्त्वा-त्याग कर, करोति करता है, यः जो, लिप्यते-लिप्त होता है, न-नहीं, सः- वह, पापेन- पाप से, पद्मपत्रम् -कमल-पत्र, इव-भाँति, अम्भसा-जल से।
अनुवाद : अनासक्त हो कर परमात्मा को समर्पित कर के कर्म करने वाला मनुष्य जल में कमल-पत्र की भाँति पाप से लिप्त नहीं होता।
व्याख्या : अध्याय IV श्लोक १८,२०,२१,२२,२३,३७,४१; अध्याय V श्लोक १०, ११ और १२ - ये सभी एक ही सत्य को उद्घाटित करते हैं। वह योगी जो कर्म-फल के प्रति आसक्ति त्याग कर, अहंकारशून्य हो कर परमात्मा को समर्पित कर के कर्म करता है, वह कर्म के बन्धन से मुक्त रहता है। उसे तो मोक्ष का अनुराग भी नहीं है। वह कर्म में अकर्म को देखता है। उसके समस्त कर्म ज्ञानाग्नि में जल जाते हैं। वह भव-बन्धन से (संसार-चक्र से) छूट जाता है। वह जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है। उसका हृदय विशुद्ध हो जाता है और उसे आत्म-ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्म-ज्ञान से वह मोक्ष प्राप्त करता है। ऊपर वर्णित १० श्लोकों का यही सार है। (निरूपण-III.30)
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ।।११ ।।
शब्दार्थ : कायेन-शरीर से, मनसा-मन से, बुद्ध्या-बुद्धि से, केवलैः केवल, इन्द्रियैः - इन्द्रियों से, अपि-भी, योगिनः-योगी, कर्म-कर्म, कुर्वन्ति-करते हैं, सङ्गम्-आसक्ति, त्यक्त्वा-त्याग कर, आत्मशुद्धये- अन्तःकरण की शुद्धि के लिए।
अनुवाद : योगी जन (कर्मयोगी) आसक्ति को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियों से आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं।
व्याख्या : योगी का अभिप्राय यहाँ कर्मयोगी से है जो कर्मयोग के पथ पर अडिग चल रहा है, अहंभाव से रहित है, निःस्वार्थ भाव से कार्य करने वाला है, फल की इच्छा को त्याग कर समर्पित भाव से कर्म करने वाला है।
केवलम् -केवल शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियों से, अहंभाव और स्वार्थभाव त्याग कर कर्म करता है।
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।।१२ ।।
शब्दार्थ : युक्तः योगी, कर्मफलम् -कर्मफल को, त्यक्त्वा-त्याग कर, शान्तिम् - शान्ति, आप्नोति-प्राप्त करता है, नैष्ठिकीम् आत्यन्तिक, अयुक्तः जो परमात्मा से एक नहीं है, कामकारेण-इच्छा से प्रेरित, फले-कर्मफल में, सक्तः- आसक्त, निबध्यते-बँधता है।
अनुवाद : योग में समन्वित युक्त पुरुष कर्मफल की आसक्ति त्याग कर (भगवत्प्राप्ति रूप) शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता है और सकाम कर्म करने वाला अयुक्त पुरुष फल की इच्छा से कर्म करता है और बन्धन में आता है।
व्याख्या : 'शान्तिं नैष्ठिकीम्' का अभिप्राय है-निष्ठा अथवा भक्ति से उत्पन्न शान्ति । समत्वभाव से युक्त पुरुष जो फल की कामना त्याग कर भगवदर्पित कर के कर्म करता है और कहता है- "मैं व्यक्तिगत लाभ हेतु कर्म नहीं करता, प्रत्युत् ईश्वर के लिए करता हूँ", वह विवेक-बुद्धि में दृढ़ता, कर्म-त्याग, ज्ञान-प्राप्ति और हृदय की शुद्धि-इन चार अवस्थाओं से प्राप्त भक्तिभाव से उद्भूत शान्ति प्राप्त करता है। किन्तु अयुक्त पुरुष जो कामनाओं के जाल में फँसा हुआ है और फल की आसक्ति रखता है और कहता है- "मैंने अमुक-अमुक कर्म किये हैं और उनका फल भी प्राप्त करूँगा", वह निस्सन्देह बन्धन में पड़ता है।
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ।।१३ ।।
शब्दार्थ : सर्वकर्माणि-समस्त कर्म, मनसा-मन से, संन्यस्य-त्याग कर, आस्ते-रहता है, सुखम् -सुखपूर्वक, वशी संयमी, नवद्वारे-नौ द्वारों वाले, पुरे-नगर में, देही देह युक्त आत्मा, न-नहीं, एव-ही, कुर्वन् -करते हुए, न-नहीं, कारयन् -कराते हुए।
अनुवाद : मन से अर्थात् आन्तरिक रूप से समस्त कर्मों का त्याग कर के, अपनी प्रकृति को संयत कर के देहधारी आत्मा (शरीर और इन्द्रियों से) न तो कर्म करता हुआ और न ही करवाता हुआ नव द्वारों वाली पुरी में सुख से निवास करता है।
व्याख्या : समस्त कर्म-
(१) नित्य कर्म-ये अपरिहार्य कर्तव्य हैं। इनके करने से कोई पुण्य तो नहीं होता; किन्तु न करने से दोष अवश्य लगता है। सन्ध्यावन्दन आदि इसी श्रेणी में आते हैं।
(२) नैमित्तिक कर्म-विशेष अवसर पर किसी निमित्त से किये जाने वाले कर्तव्य जैसे शिशु के जन्म पर अथवा ग्रहण-काल में किये जाने वाले अनुष्ठान आदि नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं।
(३) काम्य कर्म-ये कर्म अभीप्सित हैं। किसी अभिलाषा जैसे वर्षा, पुत्र-प्राप्ति आदि को ले कर किये जाने वाले
(४) निषिद्ध कर्म-चोरी करना, मदिरापान आदि कर्म निषिद्ध कर्म हैं।
(५) प्रायश्चित्त कर्म-अशुभ कर्म (पाप कर्म) का फल शून्य करने हेतु किये जाने वाले कर्म प्रायश्चित्त कर्म हैं।
जिस मनुष्य ने अपने अन्तःकरण को वश में कर लिया है, वह विवेक द्वारा सब कर्मों का त्याग कर देता है। वह कर्म में अकर्म देखता है और नव द्वार वाली इस नगरी में सुखपूर्वक रहता है; क्योंकि वह सब प्रकार के उद्वेग, चिन्ता, उत्सुकता और भय से मुक्त हो चुका है, उसका मन शान्त है और वह शाश्वत परम शान्ति में आनन्द लेता है। इस नव द्वारों की पुरी में आत्मा ही स्वामी है, राजा है और मन, इन्द्रियाँ अवचेतन मन तथा बुद्धि प्रजा हैं।
अज्ञान में पड़ा संसारी मनुष्य कहता है- "मैं आरामकुर्सी पर आराम कर रहा हूँ", देहाध्यास से ऊपर उठा व्यक्ति जिसने जान लिया है कि आत्मा पंच भौतिक शरीर से पृथक् है, कहता है-"मैं शरीर में विश्राम कर रहा हूँ।" (निरूपण-XVIII. 17, 50)
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।।१४ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, कर्तृत्वम् -कर्तापन, न -नहीं, कर्माणि-कर्म, लोकस्य इस लोक के, सृजति सृजन करता है, प्रभुः भगवान्, ननहीं, कर्मफलसंयोगम् -कर्म का फल के साथ संयोग, स्वभावः स्वभाव (प्रकृति), तु-लेकिन, प्रवर्तते-प्रवृत्त होता है।
अनुवाद : परमात्मा न तो किसी को कर्ता बनाता है और न ही किसी को कर्म के लिए प्रेरित करता है। कर्म का फल के साथ संयोग भी प्रभु नहीं करता। स्वभाव ही लोक में सब वस्तुओं में प्रवृत्त होता है।
व्याख्या : भगवान् कर्तापन का सृजन नहीं करते। वे किसी को कर्म के लिए भी प्रेरित नहीं करते। वे कभी किसी से यह नहीं कहते- "यह करो या वह करो।" वे कर्म-फल का संयोग भी नहीं करते। प्रकृति ही बरत रही है सब ओर। (निरूपण-III.33)
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।।१५ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, आदत्ते-लेता है, कस्यचित् -किसी का, पापम्पाप, ननहीं, च-और, एव-ही, सुकृतम् -पुण्य, विभुः परमेश्वर, अज्ञानेन अज्ञान के द्वारा, आवृतम् ढका है, ज्ञानम्-ज्ञान, तेन-उससे, मुह्यन्ति-मोहित होते हैं, जन्तवः - प्राणी।
अनुवाद : परमेश्वर न तो किसी के पाप कर्म का आदान (लेना) करते हैं और न ही पुण्य कर्म का। अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है; इसीलिए प्राणी भ्रमित हो जाते हैं।
व्याख्या : ज्ञान पर अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य भ्रमित हो रहा है। वह स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान कर सोचता है- "मैंने अमुक पुण्य कर्म किये हैं; अतः इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। स्वर्ग का सुख मिलेगा और समृद्ध परिवार में जन्म होगा।"
कस्यचित् -किसी का भी अर्थात् भक्त का भी।
प्रकृति और उसके कार्य (effect) शरीर, मन, प्राण अथवा जीवन-शक्ति और इन्द्रियों से एकत्व होने पर मनुष्य बन्धन में पड़ता है। हृदय में विराजित, कर्म से अतीत अमर आत्मन् से सायुज्य प्राप्त कर लेने पर वह मोक्ष प्राप्ति करता है।
जब 'मैं' कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होता, परमेश्वर पाप-पुण्य कर्म कैसे स्वीकार कर सकता है? (निरूपण-V.29)
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ।।१६ ।।
शब्दार्थ : ज्ञानेन-ज्ञान से, तु-लेकिन, तत्-वह, अज्ञानम्-अज्ञान, येषाम् -जिनका, नाशितम् - नष्ट हो गया, आत्मनः- जीव का, तेषाम् उनका, आदित्यवत् सूर्य की भाँति, ज्ञानम् - ज्ञान, प्रकाशयति-प्रकाशित होता है, तत्परम् सर्वोच्च ।
अनुवाद : आत्म-ज्ञान से जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके लिए ज्ञान सूर्य की भाँति उस परब्रह्म को प्रकाशित कर देता है।
व्याख्या : जिस प्रकार से देदीप्यमान सूर्य स्थूल भौतिक जगत् को प्रकाशमय कर देता है, उसी प्रकार मानवीय दुःखों के मूल कारण अज्ञान का आत्म-ज्ञान द्वारा विनाश होने पर यह ज्ञान सर्वोच्च सत्ता परब्रह्म को प्रकाशित करता है।
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्भूतकल्मषाः ।।१७ ।।
शब्दार्थ : तद्बुद्धयः- भगवत्परायण बुद्धि वाले, तदात्मानः-तरूप चेतना (आत्मा) वाले, तन्निष्ठाः- उसी में प्रतिष्ठित, तत्परायणाः- उसी परमेश्वर को परम लक्ष्य मानने वाले, गच्छन्ति-जाते हैं, अपुनरावृत्तिम् - अपुनरावृत्ति हेतु अर्थात् पुनः न लौटने के लिए, ज्ञाननिर्भूतकल्मषाः - ज्ञान से जिनकी अविद्या का विनाश हो गया है।
अनुवाद : जिनकी बुद्धि तद्रूप हो गयी है, जिनका मन (आत्मा) तद्रूप हो गया है, उसी में जो स्थित हो गये हैं और जिनका परम उद्देश्य उसी परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसे महापुरुष पुनः लौट कर न आने के लिए परम धाम को जाते हैं अर्थात् मोक्ष-प्राप्ति करते हैं, उनके पाप ज्ञान से धुल जाते हैं।
व्याख्या : वे अपने विचार ब्रह्म पर केन्द्रित करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि ब्रह्म ही उनका वास्तविक आत्म-तत्त्व है। सतत, अनवरत ध्यान से वे उसमें स्थित हो जाते हैं। उनके लिए नाम-रूप का यह संसार लुप्त हो जाता है। वे केवल ब्रह्म में ही वास करते हैं। उनका केवल आश्रय ब्रह्म ही है। वे आत्मा में ही आनन्दित रहते हैं। आत्मा में ही सन्तुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती; क्योंकि उनके समस्त पाप ब्रह्म-ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। (निरूपण-IX.34)
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।।१८ ।।
शब्दार्थ : विद्याविनयसंपन्ने - विद्या और विनम्रता से युक्त, ब्राह्मणे-ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनि-हाथी में, शुनि-कुत्ते में, च-और, एव-ही, श्वपाके-चाण्डाल में, च-और, पण्डिताः - ज्ञानी जन, समदर्शिनः समदर्शी ।
अनुवाद : ज्ञानीजन सुशिक्षित और विनम्र ब्राह्मण में तथा गाय में, हाथी में, शुनि (कुत्ते) में और चाण्डाल में भी समदृष्टि रखते हैं।
व्याख्या : जीवन्मुक्त अथवा ब्राह्मण सर्वत्र आत्म-तत्त्व के दर्शन करता है; अतः वह समान दृष्टि रखता है। ज्ञानी की यह महती दिव्य दृष्टि अनिर्वचनीया है। आत्मा अथवा ब्रह्म तो सर्वथा उपाधि रहित, निराकार, शुद्ध और सूक्ष्म स्वरूप है, उस पर किसी प्रकार की कोई उपाधि का प्रभाव नहीं पड़ता । सूर्य का प्रतिबिम्ब गङ्गा, सागर अथवा गन्दे नाले पर पड़े, इससे सूर्य कदापि प्रभावित नहीं होता। सूर्य में कोई अन्तर नहीं आता। ऐसा ही परमात्मा के साथ है। उपाधियाँ उसे प्रभावित नहीं करतीं। आकाश किसी पात्र में हो, कक्ष में हो अथवा मेघ आदि में हो । आकाश तो आकाश ही है। इसी भाँति ब्रह्म तो ब्रह्म ही है।
ब्राह्मण सात्त्विक है, गाय राजसिक है तथा हाथी, कुत्ता और चाण्डाल तामसिक है। ज्ञानी सब में उसी एक आत्मा का दृष्टिकोण रखते हैं जो तीन गुणों और उनके स्वभाव से अतीत है। (निरूपण - VI.8, 32; XIV.24)
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ।।१९ ।।
शब्दार्थ : इह-यहाँ, एव-ही, तैः-उनके द्वारा, जितः- जीता गया है, सर्गः पुनर्जन्म अथवा संसार, येषाम् - जिनका, साम्ये-साम्यावस्था में, स्थितम् -स्थित, मनः-मन, निर्दोषम् - दोष रहित, हि-निश्चय से, समम् समान, ब्रह्म-ब्रह्म, तस्मात्-इसलिए, ब्रह्मणि-ब्रह्म में, तेवे, स्थिताः- स्थित हैं।
अनुवाद : इस संसार में भी जन्म-मृत्यु पर विजय वही प्राप्त कर सकते हैं जिनका मन साम्यावस्था में स्थित है। ब्रह्म तो समदृष्टि है, निश्चित रूप से निर्दोष है; इसीलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं।
व्याख्या : मन की साम्यावस्था आने पर मनुष्य जन्म-मृत्यु पर विजयी हो जाता है। वह बन्धन-मुक्त हो कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मन जब पूर्ण रूप से समान दृष्टि हो जाता है, तब वह ब्रह्म-साक्षात्कार करता है।
ब्रह्म सदा निरंजन है और उपाधि रहित है; इसीलिए वह कुत्ते और चाण्डाल आदि में भी रहने पर उनसे प्रभावित नहीं होता। अतः वह निर्विकार है, दोष रहित है। वह एक है और सब में समान रूप से प्रतिष्ठित है।
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ।।२० ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, प्रहृष्येत् -प्रसन्न हो, प्रियम् -प्रिय को, प्राप्य-प्राप्त कर के, न-नहीं, उद्विजेत्-दुःखी हो, प्राप्य-प्राप्त कर के, च-और, अप्रियम् - अप्रिय (वस्तु) को, स्थिरबुद्धिः - स्थिर बुद्धि वाला, असम्मूढः- असंभ्रमित, ब्रह्मवित् - ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मणि-ब्रह्म में, स्थितः - स्थित ।
अनुवाद : अभेद रूप से ब्रह्म में स्थित, ब्रह्मवेत्ता, जो अकिंकर्तव्यविमूढ़ तथा स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा पुरुष प्रिय पदार्थ की प्राप्ति पर आनन्द नहीं मनाता और अप्रिय को प्राप्त कर के उद्विग्न नहीं होता।
व्याख्या : यहाँ ब्रह्मज्ञानी की अवस्था वर्णित है। जिसने ब्रह्म के साथ एकत्व स्थापित कर लिया है, वह सदा समभाव रहता है, भ्रमित नहीं होता। ब्रह्म में आश्रित होने के कारण उसने समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है। जिसका मन चंचल है और जिसने स्वयं को शरीर और मन से एकरूप कर लिया है, वह सुख-दुःख की अनुभूति करता है, प्रिय वस्तु की प्राप्ति पर हर्षित होता है और अप्रिय की प्राप्ति पर दुःखी होता है । (निरूपण-VI.21,27,28;XIII.12 XIV.20)
बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ।।२१ ।।
शब्दार्थ : बाह्यस्पर्शेषु-बाह्य सम्पर्कों में, असक्तात्मा-अनासक्त मन वाला, विन्दति-प्राप्त करता है, आत्मनि-आत्मा में, यत्-जो, सुखम् सुख, सः-वह, ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्म के योग में युक्त आत्मा, सुखम् -सुख, अक्षयम् -कभी समाप्त न होने वाला, अश्नुते-प्राप्त करता है।
अनुवाद : जिसका चित्त बाह्य विषयों में अनुरक्त नहीं है, वह अपनी आत्मा में ही आनन्द से रहता है। एकाग्रचित्त हो कर परमात्मा के ध्यान में मग्न साधक अक्षय सुख को प्राप्त करता है।
व्याख्या : बाह्य विषयों में अनासक्त चित्त और ब्रह्म में एकाग्रचित्त वाला साधक अपनी आत्मा में ही दिव्य आनन्द का उपभोग करता है।
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ।।२२ ।।
शब्दार्थ : ये-जो, हि-निश्चयेन, संस्पर्शजाः-स्पर्श से समुद्भूत, भोगाः - भोग (सुख), दुःखयोनयः - दुःख देने वाले, एव-ही, ते-वे, आद्यन्तवन्तः- आदि और अन्त सहित, कौन्तेय-कुन्ती-पुत्र अर्जुन, न-नहीं, तेषु उनमें, रमते- आनन्द लेता है, बुधः - बुद्धिमान्।
अनुवाद : बाह्य संस्पर्श (इन्द्रिय-विषयों के संयोग) से उत्पन्न सुख तो हे अर्जुन, मात्र दुःख का हेतु है; क्योंकि उनका आदि भी है और अन्त भी है अर्थात् वे नित्य नहीं हैं। इसी कारण विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ।
व्याख्या : मनुष्य सुख की खोज में भटकता है और बाह्य नश्वर पदार्थों में इसे ढूँढ़ता है। सुख प्राप्त करने की अपेक्षा वह अपने ऊपर दुःखा का भार ही वहन कर लाता है।
ऐन्द्रिक-विषयों से मुख मोड़ लो। उनमें किंचित् मात्र भी सुख का आभास नहीं है। आनन्दस्वरूप अमर आत्मा में अन्तःकरण को लगा दो। इन्द्रियों के विषय तो सादि और सान्त हैं। उनका वियोग दुःख का कारण है। आदि और अन्त के मध्य काल में मनुष्य क्षणिक, मिथ्या निःसत्त्व सुख का अनुभव करता है। यह क्षणिक सुख अज्ञान के कारण है। दूसरे लोक में भी यही अनुभव होगा। विवेकी अथवा आत्मज्ञानी इन्द्रिय-सुखों में आनन्द नहीं लेगा। केवल अज्ञानी ही इनमें सुख का आभास करता है। (निरूपण - II.14; XVIII.38)
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ।।२३ ।।
शब्दार्थ : शक्नोति-समर्थ है, इह-यहाँ (इस जगत् में), एव-ही, यः-जो, सोढुम् -सहन करने में, प्राक् -पूर्व, शरीरविमोक्षणात् - शरीर त्यागने से, कामक्रोधोद्भवम् -क्रोध और कामना से उद्भूत, वेगम्-वेग को, सः-वह, युक्तः समाहित, सः वह, सुखी-सुखी, नरः- मनुष्य ।
अनुवाद : इसी लोक में जो मनुष्य शरीर त्याग करने से पूर्व इच्छा और क्रोध से उद्धत वेग को सहन करने में समर्थ है, वह योगी है, वह सुखी है।
व्याख्या : 'युक्त' का अभिप्राय है- समन्वित अथवा योग में दृढ़ संकल्प वाला अर्थात् आत्मस्थ ।
कामना और क्रोध शान्ति के प्रबल शत्रु हैं। इन्हें मारना अत्यन्त कठिन है। इन शत्रुओं के विनाश के लिए प्रबल प्रयास करना होगा।
साधारण अर्थ में काम सब प्रकार की इच्छाओं के लिए प्रयुक्त होता है। विशेष अर्थ में यह कुवासना अथवा रताभिलाषा है।
इहैव का अर्थ है-इसी जीवन-काल में। कामेच्छा मन का संक्षोभ है जो रोमांच से और प्रसन्न वदन से प्रतिभासित होता है। क्रोध का वेग मन की उस विफलता की ओर संकेत करता है जो आग्नेय (लाल) नेत्रों से, स्वेद से, होंठ काटने से और शरीर के कम्पन से ज्ञात होता है (झलकता है)। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि संसार में सर्वाधिक सुखी मनुष्य वही है जिसने इच्छा और क्रोध पर विजय पा ली है। विपुल सम्पत्ति, सुन्दर स्त्री और सुन्दर बच्चे सुख प्रदान नहीं कर सकते । अतः पूर्ण शक्ति लगा कर इच्छा और क्रोध को समूल नष्ट कर डालो; क्योंकि ये शाश्वत आनन्द के शत्रु हैं।
काम (इच्छा) किसी सुखद और अनुकूल पदार्थ को प्राप्त करने की आकाङ्क्षा है जो सुख प्रदान करती है और जो दृश्य, श्रव्य अथवा स्मरणीय है। क्रोध किसी दुःखद और प्रतिकूल वस्तु के प्रति प्रतिरोध है जो पीड़ा पहुँचाने वाला है और दृश्य, श्रव्य अथवा स्मरणीय है।
योगी काम एवं क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग पर नियंत्रण कर लेता है, राग और द्वेष अथवा रुचियों एवं अरुचियों के संवेग को नष्ट कर देता है तथा अपने अन्तरतम में स्थित रहता हुआ मन की समता को प्राप्त कर लेता है, अतः वह सदैव प्रसन्न रहता है। (निरूपण - VI.18)
योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव यः ।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।।२४ ।।
शब्दार्थ : यः-जो, अन्तःसुखः - भीतर से सुखी, अन्तरारामः - अन्तर में रमण करने वाला, तथा-और, अन्तज्योंतिः- भीतर से देदीप्यमान, एव-ही, यः-जो, सः-वह, योगी-योगी, ब्रह्मनिर्वाणम् -मोक्ष, ब्रह्मभूतः-स्वरूपसिद्ध हो कर, अधिगच्छति-प्राप्त करता है।
अनुवाद : जो मनुष्य अपनी अन्तरात्मा में आह्लादित है, अन्तःकरण में ही रमण करता है और जिसने अपने भीतर ही ज्योति प्राप्त कर ली है, ऐसा योगी ब्रह्मस्वरूप हो कर निर्वाण प्राप्त करता है।
व्याख्या : 'अन्तः' का अभिप्राय है- आत्मा में। वह ब्रह्मनिर्वाण अथवा मोक्ष इसी जन्म में प्राप्त करता है। वह जीवन्मुक्त बन जाता है।
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।।२५ ।।
शब्दार्थ : लभन्ते-प्राप्त करते हैं, ब्रह्मनिर्वाणम् -परम आनन्द को, ऋषयः-ऋषि, क्षीणकल्मषाः - जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, छिन्नद्वैधाः- जिनके द्वैत (संशय) छिन्न-भिन्न हो गये हैं, यतात्मानः-संयमी, सर्वभूतहिते-समस्त प्राणियों के कल्याण में, रताः-संलग्न ।
अनुवाद : वे ऋषि परम आनन्द की अनुभूति करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं जिनके समस्त पाप नष्ट हो गये हैं, द्वैत (संशय) छिन्न-भिन्न हो गये हैं और जो मनसा अनुशासित हैं, संयमी हैं और सब प्राणियों के कल्याण में आनन्द लेते हैं।
व्याख्या : अग्निहोत्र (दैनिक यज्ञादि अनुष्ठान) तथा अन्य यज्ञ निष्काम भाव से करने पर पाप क्षीण होते हैं (देखें - III.13) । अद्वैत ब्रह्म में सतत ध्यान से कर्म समाप्त होते हैं। ऐसा महापुरुष मनसा, वाचा, कर्मणा किसी को हानि नहीं पहुँचाता; क्योंकि वह परोपकार में लगा हुआ है और सबमें स्वात्मा के दर्शन करता है। (निरूपण –XII.4)
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ।। २६ ।।
शब्दार्थ : कामक्रोधवियुक्तानाम् -काम-क्रोध से विमुक्त, यतीनाम् - आत्म-संयत तपस्वियों का, यतचेतसाम् - जिन्होंने अपने विचारों को संयत कर लिया है, अभितः-सब ओर से, ब्रह्मनिर्वाणम्-आत्म-साक्षात्कार, वर्तते-होता है, विदितात्मनाम् - आत्म-ज्ञानियों का ।
अनुवाद : सब ओर से आनन्द की वृष्टि उन तपस्वियों पर होती है जो आत्म-संयमी हैं, जिन्होंने काम-वासनाओं और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विचारधारा (मन) को वश में कर लिया है और आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
व्याख्या : वे पुरुष, जिन्होंने श्रवण (शास्त्रों को सुनना), मनन (आत्म-चिन्तन), निदिध्यासन (ध्यान) का अभ्यास निष्काम भाव से किया है, जो ब्रह्म में स्थित हैं, आत्म-ज्ञान के प्रति दृदसंकल्प हैं, वे कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कर्मयोग से क्रम-मुक्ति का प्रसाद मिलता है, पहले मन की शुद्धि, फिर ज्ञान, कर्मों का त्याग और अन्ततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।
स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे ध्रुवोः ।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।। २७ ।।
शब्दार्थ : स्पर्शान् बाह्य विषयों को, कृत्वा-कर के, बहिः- बाहर, बाह्यान् बाहर के, चक्षुः - नेत्र (दृष्टि), च-और, एव-ही, अन्तरे-मध्य में, ध्रुवोः - भौंहों के, प्राणापानौ-नासिका के भीतर चलने वाले और बाहर जाने वाले प्राण और अपान वायु, समौ-समान, कृत्वा-कर के, नासाभ्यन्तरचारिणौ-नासिकाओं के भीतर चलने वाले ।
अनुवाद : शब्दादि बाह्य विषयों को बाहर ही रोक कर, दृष्टि को भ्रूमध्य पर केन्द्रित कर, नथुनों में चलने वाली प्राण और अपान वायु को रोक कर,
व्याख्या : श्लोक २७ और २८ ध्यानयोग से सम्बद्ध हैं। बाह्य विषय हैं- ध्वनि तथा अन्य इन्द्रिय-विषय। यदि मन बाह्य विषयों का चिन्तन न करे, तो वे मन से लुप्त हो जाते हैं। इन्द्रियाँ ही द्वार हैं जिनके द्वारा ध्वनि आदि इन्द्रियों के विषय मन में प्रवेश करते हैं।
यदि दृष्टि को भ्रूमध्य पर एकाग्रित किया जाये, तो नेत्र गोलक अचल और स्थिर हो जाते हैं। लयबद्ध श्वास ली जाती है। श्वास को तालबद्ध करना होगा। ऐसा करने से मन स्थिर हो जाता है। श्वास के लयबद्ध होने से मन तथा समस्त प्रणाली में समत्व आ जाता है। (निरूपण –VI.10, 14; VIII.10)
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ।।२८ ।।
शब्दार्थ : यतेन्द्रियमनोबुद्धिः - जिसकी इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि (सदा) संयत हों, मुनिः योगी, मोक्षपरायणः- मोक्ष ही जिसका परम लक्ष्य हो, विगतेच्छाभयक्रोधः- इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त, यः-जो, सदा-सदा, मुक्तः मुक्त, एव-निश्चय से, सः वह ।
अनुवाद : इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि को संयत कर, मोक्षपरायण अर्थात् मोक्ष ही जिसका परम लक्ष्य है और जिसने इच्छा, भय और क्रोध को विजित कर लिया है, ऐसा योगी निश्चित रूप से सदा मुक्त है।
व्याख्या : इच्छा, भय और क्रोध पर विजय पा लेने पर मनुष्य पूर्ण मानसिक शान्ति प्राप्त करता है। इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि को वशीभूत कर के मुनि सतत ध्यानमग्न रहता है और परम आनन्द की प्राप्ति करता है।
काम, क्रोध और भय की वृत्तियाँ जागृत होने पर मन अशान्त हो जाता है। कामना रहित होने पर मन स्वतः ही भगवान् की ओर उन्मुख होता है। मोक्ष उसका सर्वोच्च लक्ष्य बन जाता है।
मुनि वह है जो मनन, आत्म-विश्लेषण और ध्यान करता है।
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।।२९ ।।
शब्दार्थ : भोक्तारम् - उपभोग करने वाला, यज्ञतपसाम् यज्ञों और तपों का, सर्वलोकमहेश्वरम् -सब लोकों का महेश्वर, सुहृदम् -मित्र, सर्वभूतानाम् - सब प्राणियों का, ज्ञात्वा-जान कर, माम्-मुझे, शान्तिम्-शान्ति, ऋच्छति -प्राप्त करता है।
अनुवाद : जो साधक मुझे सब यज्ञों और तपों का उपभोग करने वाला, समस्त लोकों का महान् से भी महानतम ईश्वर और सभी प्राणियों का हितचिन्तक मित्र-इस प्रकार से जानता है, वह शान्ति प्राप्त करता है।
व्याख्या : मैं समस्त यज्ञादि और तपों का स्वामी हूँ। मैं ही उनका सृजनकर्ता, लक्ष्य और उनका महेश्वर हूँ। मैं सब प्राणियों का मित्र हूँ। प्रतिफल की आशा किये बिना उनका कल्याण करता हूँ। मैं ही उनके समस्त कर्मफल का प्रणेता हूँ। उनके मन, विचार और कर्मों का मौन साक्षी हूँ; क्योंकि मैं उनके अन्तःकरण में वास करता हूँ। मुझे प्राप्त कर लेने पर वे भवबन्धन से मुक्त हो जाते हैं, जागतिक कष्ट-पीड़ा से छुटकारा पा कर वे परम शान्ति प्राप्त करते हैं। (निरूपण -V.15; IX.24)
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।।५ ।। ।।
इति कर्मसंन्यासयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ षष्ठोऽध्यायः
ध्यानयोगः
श्री भगवानुवाच
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ।।१ ।।
शब्दार्थ : अनाश्रितः - निर्भर न हो कर, कर्मफलम् -कर्मफल (पर), कार्य कर्म-कर्तव्य कर्म, करोति-करता है, यः- जो, सः- वह, संन्यासी संन्यासी, च-और, योगी-योगी, च-और, ननहीं, निरग्निः- यज्ञादि न करने वाला, न-नहीं, च-और, अक्रियः- (धार्मिक) अनुष्ठान न करने वाला।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : कर्मफल पर आश्रित न रह कर, फल की इच्छा त्याग कर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है वही संन्यासी है और वही योगी है। अग्नि का और कर्म का त्याग करने वाला संन्यासी नहीं है।
व्याख्या : फल की इच्छा त्याग कर अग्निहोत्र आदि क्रियाएँ करने से मन शुद्ध होता है और ध्यानयोग के लिए साधन बनता है।
कार्यं कर्म-कर्तव्य कर्म।
निरग्निः - बिना अग्नि के। जिसने अग्निहोत्र आदि दैनिक क्रियाओं का त्याग कर दिया है जो अग्नि की सहायता से की जाती हैं। अक्रियः - बिना कर्म जिसने तपस् तथा अन्य परोपकार के कार्य जैसे धर्मशाला (विश्रामगृह) का निर्माण, धर्मार्थ चिकित्सालय का निर्माण, कुआँ खुदवाना, निर्धन को भोजन देना आदि, त्याग दिये हैं।
संन्यासी-जिसने कर्मफल की इच्छा का त्याग कर दिया है।
योगी-स्थिरधीः । ये दोनों शब्द यहाँ गौण अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, वस्तुतः उसे संन्यासी अथवा योगी अभिहित करने के लिए नहीं। संन्यासी न तो अग्निहोत्र करता है, न ही अन्य क्रियाएँ । किन्तु वास्तविक त्याग के बिना इन्हें (अग्निहोत्र और कर्म) त्यागना सच्चा संन्यास नहीं है।
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव ।
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ।।२।।
शब्दार्थ: यम् -जिसे, संन्यासम्-संन्यास, इति-इस प्रकार, प्राहुः-कहते हैं, योगम् योग, तम्-उसे, विद्धि-जानो, पाण्डव-हे पाण्डव, न-नहीं, हि-निश्चयेन, असंन्यस्तसंकल्पः - जिसने अपने संकल्पों (विचारों) का त्याग नहीं किया, योगी-योगी, भवति-होता है, कश्चन-कोई भी।
अनुवाद : हे अर्जुन, संन्यास ही योग है, ऐसा जानो । वस्तुतः संकल्पों का संन्यास (त्याग) किये बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ।
व्याख्या : भविष्य की योजनाएँ बना कर उनके परिणाम का अनुमान करने वाली मन की विचारणा-शक्ति की क्रिया को संकल्प कहा जाता है। योजनाएँ बना कर कर्मफल की आकाङ्क्षा करने वाला कभी कर्मयोगी नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति, जो कर्म में आस्था रखता है, फल की इच्छा के त्याग बिना स्थिरचित्त योगी नहीं बन सकता। फल का विचार ही निश्चित रूप से मन को अशान्त करता है।
भगवान् कृष्ण कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं; क्योंकि कर्मयोग ध्यानयोग के लिए साधनस्वरूप अथवा बहिरङ्गयोग है। कर्मयोग ध्यानयोग के सोपान की सोपान-शिला है। समय आने पर यह ध्यानयोग में प्रवृत्त करता है। कर्मयोग के अभ्यास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन हेतु कहा गया है कि कर्मयोग भी संन्यास है। (निरूपण-V.4)
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ।।३ ।।
शब्दार्थ : आरुरुक्षोः- आरूढ़ होने की इच्छा वाला, मुनेः मुनि का, योगम् योग, कर्म-कर्म, कारणम् -कारण, उच्यते-कहा जाता है, योगारूढस्य-जिसने योग प्राप्त कर लिया है, तस्य-उसके लिए, एव-ही, शमः -शान्ति को, कारणम् -कारण, उच्यते-कहा गया है।
अनुवाद : योगारूढ़ होने के इच्छुक मुनि के लिए निष्काम कर्म ही साधन बताया गया है, किन्तु योग प्राप्ति के उपरान्त उसी मुनि के लिए शम अर्थात् सब कर्मों का अभाव ही साधन बताया गया है।
व्याख्या : योगारूढ़ होने के जिज्ञासु के लिए जो दीर्घावधि तक न तो ध्यान में बैठ सकता है और न ही स्थिरबुद्धि हो सकता है, कर्म ही साधन बताया है। कर्म से मन पवित्र होता है और स्थिरतापूर्वक अभ्यास के लिए अनुकूल हो जाता है। निष्काम कर्म से स्थिर (अविचल) एकाग्रता और ध्यान में सहायता मिलती है।
जो साधक योगारूढ़ हो चुका है, उसके लिए शम अथवा कर्म का त्याग (निष्काम कर्म) ही साधन है।
जितना अधिक कुशलता से वह कर्म का त्याग करता है, उतना अधिक स्थिर उसका मन होता है और उतनी शान्ति उसे प्राप्त होती है। अब वह सहज रूप से मन को आत्मा में स्थित कर सकता है। "एक ब्राह्मण के लिए आत्मैक्य, सत्य, सच्चरित्र, स्थिरता, समत्व, सरलता और सर्वकर्मत्याग के समान सम्पदा नहीं है।" (महाभारत, शान्ति-पर्व, १७५.३८)
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ।
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।।४ ।।
शब्दार्थ : यदा-जब, हि-निश्चित रूप से, न-नहीं, इन्द्रियार्थेषु - इन्द्रियों के विषयों में, 7-7 hat 6t . कर्मसु-कर्मों में, अनुषज्जते-आसक्त होता है, सर्वसंकल्पसंन्यासी-समस्त संकल्पों का परित्यक्ता, योगारूढः- योगनिष्ठ, तदा-तब, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : समस्त संकल्पों का त्याग कर देने पर जब मनुष्य की इन्द्रिय-विषयों अथवा कर्मों में अनुरक्ति नहीं रह जाती, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है।
व्याख्या : योगारूढ़-योग में स्थित । मन को पूर्णरूपेण स्थिर करके, इन्द्रिय-विषयों से इसे पराङ्मुख कर के, कर्मों का अनुराग त्याग कर (see notes on कर्म - V.13) ध्वनि आदि तन्मात्राओं की आसक्ति त्याग कर, उनकी निरर्थकता को जान कर जब कोई योगी सब संकल्पों का भी त्याग कर देता है और जान लेता है कि यही संकल्प सांसारिक विषयों के प्रति विविध कामनाएँ जाग्रत करते हैं तभी वह योगारूढ़ कहलाता है।
विषयों का चिन्तन मत करो। इच्छाएँ स्वयं ही मर जायेंगी। विषय-चिन्तन से मुक्त कैसे हों? आत्म-चिन्तन करो। भगवद्-चिन्तन करो। तभी विषयों के चिन्तन से मुक्ति मिल सकती है।
संकल्प-त्याग का अभिप्राय है-सब इच्छाओं और (सकाम) कर्मों का त्याग करना; क्योंकि सभी इच्छाएँ संकल्प से उत्पन्न होती हैं। मनुष्य पहले सोचता है, फिर आकाङ्क्षित वस्तु की प्राप्ति का साधन करता है।
"पुरुष जैसी कामना वाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है और जैसे संकल्प वाला होता है, वैसा ही कर्म करता है।" (बृहदारण्यक उपनिषद्, ४.४.५)
सर्वकर्म परित्याग का भाव इच्छाओं के परित्याग से आता है।
"हे काम! मैं जानता हूँ तुम्हारा मूल कहाँ है। तुम संकल्प (विचार) से उद्भूत हो। मैं तुम्हारा चिन्तन नहीं करूँगा और तुम्हारा अस्तित्व समूल नष्ट हो जायेगा।" (महाभारत, शान्ति-पर्व, १७७.२५)
"वस्तुतः इच्छा, विचार (संकल्प) से उत्पन्न होती है और विचार से यज्ञ उत्पन्न होते हैं।" (मनुस्मृति, II.2- काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ।।)
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।।५ ।।
शब्दार्थ : उद्धरेत् - उद्धार करो (ऊपर उठाओ), आत्मना-आत्मा के द्वारा, आत्मानम् - आत्मा का, न-नहीं, आत्मानम्-आत्मा का, अवसादयेत् -पतन करो, आत्मा-आत्मा, एव-ही, हि-वस्तुतः, आत्मनः- आत्मा का, बन्धुः-मित्र, आत्मा-आत्मा, एव-ही, रिपुः-शत्रु, आत्मनः- आत्मा का।
अनुवाद : आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उद्धार करो। इसका पतन मत होने दो। आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है।
व्याख्या : योगाभ्यास करो। मन और इन्द्रियों को नियन्त्रित करो। स्वयं का उत्थान करो और योगारूढ़ हो जाओ। योग को सुलभ करो। जीवन्त (शक्तियुक्त, क्रियाशील) योगी की भाँति यशस्वी बन कर चमको । संसार-सागर में अपना अधःपतन मत करो। आवागमन के भँवर में मत फँसो । सांसारिक मानसिकता वाले व्यक्ति मत बनो। काम, लोभ और क्रोध के दास मत बनो। सांसारिकता से ऊपर उठो । दिव्य बनो। ब्रह्मत्व प्राप्त करो।
केवल तुम स्वयं ही अपने मित्र हो । अपने शत्रु भी तुम स्वयं ही हो। सांसारिक मित्र तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है; क्योंकि वह तुममें अनुरक्त है, तुम्हारा समय व्यर्थ करता है और तुम्हारे मार्ग में बाधाएँ डालता है। वह नितान्त स्वार्थी है। तुमसे कुछ लेने के भाव से ही वह तुमसे मित्रता करता है। निज स्वार्थ की वस्तु तुमसे प्राप्त न होने पर वह तुम्हारा त्याग कर देता है। इसीलिए वास्तव में वह तुम्हारा शत्रु ही है। स्नेहवश अथवा भ्रमवश तुम अपने मित्र में आसक्त हो, तो यह तुम्हारे लिए संसार में बन्धन का कारण बनेगा।
मित्र और शत्रु बाहर नहीं हैं। वे मन में ही वास करते हैं। मन ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाता है। अतः आत्मा ही मनुष्य का बन्धु है और आत्मा ही शत्रु है। अशुद्ध मन तुम्हारा वास्तविक शत्रु है; क्योंकि यह तुम्हें संसार में बाँधता है और शुद्ध सात्त्विक मन तुम्हारा मित्र है; क्योंकि यह तुम्हें मोक्ष-प्राप्ति में सहायक है।
बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ।।६ ।।
शब्दार्थ : बन्धुः-मित्र, आत्मा-आत्मा, आत्मनः- आत्मा का, तस्य- उसका, येन-जिसके द्वारा, आत्मा-आत्मा, एव-ही, आत्मना-आत्मा के द्वारा, जितः- जीता गया है, अनात्मनः - जिसने आत्मा को नहीं जीता, तु-लेकिन, शत्रुत्वे-शत्रुभाव में, वर्तेत-रहता है (वर्तता है), आत्मा-आत्मा, एव-ही, शत्रुवत् - शत्रु की भाँति ।
अनुवाद : आत्मा, आत्मा का बन्धु उसके लिए है जिसने आत्मा से ही आत्मा को विजित कर लिया है। जिसने स्वयं पर नियन्त्रण प्राप्त नहीं किया उसके लिए आत्मा शत्रुभाव में रह कर बाह्य शत्रु की तरह व्यवहार करता है।
व्याख्या : निम्न मन पर विजय प्राप्त करो उच्चतर मन के द्वारा। निम्नतर मन तुम्हारा शत्रु है। उच्चतर मन तुम्हारा मित्र है। उच्चतर मन से मित्रता करने पर तुम निम्नतर मन को सहज ही वश में कर सकते हो। निम्नतर मन रजस् और तमस् से परिपूर्ण है। उच्च्तर मन सात्त्विक भाव से पूर्ण है।
इन्द्रियाँ, मन और आत्मा को नियन्त्रित रखने वाला ही आत्मा का बन्धु है। किन्तु यही आत्मा उसके लिए शत्रु बन जाता है जिसने अपने निम्नतर मन और इन्द्रियों को वश में नहीं किया। बाह्य शत्रु की भाँति वह उसे हानि पहुँचाता है। निम्नतर मन उसे मानो निर्दयता से घायल कर देता है। सर्वोच्च आत्मा मूल आत्मा है। मन भी आत्मा है; किन्तु गौण आत्मा है।
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ।।७ ।।
शब्दार्थ : जितात्मनः स्वयं पर विजय पाने वाले का, प्रशान्तस्य- शान्तचित्त वाले का, परमात्मा-परमात्मा, समाहितः-समाधि में स्थित (सम्यक् प्रकार से स्थित), शीतोष्णसुखदुःखेषु सरदी-गरमी, सुख-दुःख में, तथा -और भी , मानापमानयोः मान और अपमान में।
अनुवाद : जितेन्द्रिय और प्रशान्त पुरुष की सर्वोच्च आत्मा सदा समाधिस्थ रहती है। वह सरदी-गरमी, सुख-दुःख और मान-अपमान में भी सम रहता है। (ये सभी द्वन्द्व उसे प्रभावित नहीं करते)।
व्याख्या : जितेन्द्रिय योगी जो समाधि में स्थित है, वह द्वन्द्वों के विरोधी युग्मों (द्वन्द्वों) में शान्त रहता है। शीतोष्ण, दुःख-सुख, मानापमान से वह अतीत रहता है। इन्द्रियाँ वशीभूत हों, मन समाहित (सम) हो, योगी हर अवस्था में शान्तचित्त हो, विपरीत द्वन्द्वों से प्रभावित न हो, समस्त कर्मों का त्याग कर दिया हो, तभी परमात्मा वस्तुतः उसका अपना आत्मा बन जाता है। वह भगवद्-साक्षात्कार कर लेता है। आत्मस्थ (आत्मा में स्थित, समाधिस्थ) होने के कारण वह सदा सौम्य और प्रशान्त बना रहता है। प्रकृति की विपरीत परिस्थितियों में वह चट्टान की भाँति दृढ़ रहता है, उसे प्रकृति प्रभावित नहीं करती।
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।।८।।
शब्दार्थ : ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा-ज्ञान-विज्ञान से तृप्त, कूटस्थः-अविचलित, विजितेन्द्रियः - इन्द्रियों को जीतने वाला, युक्तः समन्वित, इति-इस प्रकार, उच्यते-कहा जाता है, योगी-योगी, समलोष्टाश्मकाञ्चनः - मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण खण्ड जिसके लिए समान हों।
अनुवाद : अपने ज्ञान और विज्ञान (आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म-ज्ञान) से जिस योगी की आत्मा तृप्त है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है और जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर अथवा स्वर्ण खण्ड समान हैं, वह युक्त योगी है (जिसने निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली है)।
व्याख्या : ज्ञान का अभिप्राय है-परोक्ष ज्ञान अथवा सैद्धान्तिक ज्ञान जो शास्त्राध्ययन से अर्जित किया है। विज्ञान, विशेष ज्ञान है जिसे अपरोक्ष ज्ञान (direct knowledge) भी कहते हैं। यह अनुभव से प्राप्त आत्म-ज्ञान है।
'कूटस्थ' का अर्थ है-स्थूणा (लौह-खण्ड, जिस पर लुहार कूटता है) की भाँति अपरिवर्तनशील। स्थूणा पर विभिन्न प्रकार के लौह-खण्ड, आकार बनाने के लिए हथौड़े से कूटे जाते हैं, किन्तु स्थूणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; इसी प्रकार इन्द्रिय-विषयों के सम्पर्क में आने पर भी योगी अप्रभावित रहता है, अतः कूटस्थ कहलाता है। ब्रह्मन् का दूसरा नाम कूटस्थ है जो मन की वृत्तियों का मौन साक्षी है। (निरूपण –V.18; VI.18)
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।।९ ।।
शब्दार्थ : सुहत् - शुभचिन्तक, मित्र-मित्र, अरिः-शत्रु, उदासीन- तटस्थ, मध्यस्थ-निष्पक्ष, द्वेष्य-द्वेष करने वाले, बन्धुषु सम्बन्धियों में, साधुषु साधुओं में, अपि-भी, च-और, पापेषु पापियों में, समबुद्धिः-समान भाव रखने वाला, विशिष्यते-सर्वश्रेष्ठ है।
अनुवाद : जो मनुष्य शुभचिन्तकों, मित्रों, शत्रुओं, तटस्थों, मध्यस्थों, घृणा करने वालों, सम्बन्धियों, साधुओं और पापियों में समभाव रखता है, वह सर्वश्रेष्ठ है।
व्याख्या : विशिष्यते-योगारूढ़ों में सर्वश्रेष्ठ ।
समबुद्धि-मन का समत्व । समबुद्धि योगी समान दृष्टिकोण (समदृष्टि) वाला होता है। वह निष्पक्ष होता है। सबमें समान होता है। वह जाति-भेद, वर्ण-भेद से परे होता है। निज आत्मा के समान ही सबमें समभाव रखता है। वह आत्मा में स्थित रहता है।
सुहृद्-परोपकारी मनुष्य जो निष्कामभाव से सेवा करता है और बदले में कोई आकाङ्घा नहीं रखता।
उदासीन-निरपेक्ष, तटस्थ, निरभिलाष ।
मध्यस्थ-दो विवादी जनों में मौन साक्षी रहने वाला।
साधुषु जो शुभ कर्म करते हैं और शास्त्र की आज्ञा में चलते हैं, वे साधु कहलाते हैं।
पापेषु पापी वे हैं जो अशुभ और निषिद्ध कर्म करते हैं और शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं तथा दूसरों को हानि पहुँचाते हैं।
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।।१०।।
शब्दार्थ : योगी-योगी, युञ्जीत-मन को स्थिर करे, सततम् - अविराम, आत्मानम् आत्मा को, रहसि एकान्त में, स्थितः-रह कर, एकाकी अकेला, यतचित्तात्मा-आत्मवशी (देह और मन को वश में करके), निराशी:-इच्छा रहित, अपरिग्रहः लालसा रहित।
अनुवाद : योगी को चाहिए कि वह एकान्त में अकेले रह कर मन और शरीर को नियन्त्रित कर के आशाशून्य हो कर, लालसा त्याग कर (अपरिग्रह का पालन करते हुए) अविराम परमात्मा में मन को स्थिर करने का प्रयास करे ।
व्याख्या : निर्वाण-मार्ग पर चलने वाला योगी किसी पर्वत-गुहा में ध्यानाभ्यास कर सकता है। सब प्रकार के संग्रह का उसे परित्याग कर देना उचित है।
यौगिक प्रवृत्ति और आध्यात्मिक जिज्ञासा रखने वाले गृहस्थ को चाहिए कि वह अपने ही भवन के किसी एकान्त कक्ष में ध्यान का अभ्यास करे अथवा किसी पावन नदी के तट पर (अवकाश-काल में अथवा वर्ष पर्यन्त, यदि वह अपने कार्य से सेवा-निवृत्त हो चुका है) अभ्यास करे ।
अभ्यास अविराम अनिवार्य है। अचिरेण निश्चित रूप से आत्म-ज्ञान की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है। जो मनुष्य बीच-बीच में अभ्यास छोड़ देता है और पुनः कुछ क्षणों के लिए ध्यान में बैठता है, वह अनुकूल परिणाम नहीं पा सकता । यौगिक साधक आशा, आकाङ्घा और लालसा से मुक्त हो, तभी उसका मन स्थिर हो सकता है। आशा, तृष्णा और लोभ मन को सदा अशान्त और क्षुब्ध रखते हैं। वे शान्ति और आत्म-ज्ञान के शत्रु हैं। साधक के पास अधिक संग्रह भी नहीं होना चाहिए। शरीर के निर्वाह के लिए नितान्त आवश्यक वस्तुएँ ही रखना उससे अपेक्षित है। अधिक वस्तु-संग्रह होने से मन उन्हीं का चिन्तन करेगा और उनके रक्षण की चिन्ता भी करेगा।
मनुष्य यदि प्रत्याहार, शम, दम (इन्द्रियनिग्रह और मनोनिग्रह) में भलीभाँति स्थित है, इन्द्रियाँ पूर्ण रूप से उसके आधीन हैं, तो बड़े शहर के भीड़ और शोरगुल वाले स्थान में भी वह पूर्ण एकान्त और शान्ति का अनुभव कर सकता है।
इन्द्रियाँ यदि चंचल हैं, उन्हें अन्तर्मुखी करने की शक्ति यदि व्यक्ति में नहीं है, तो हिमालय की एकान्त गुफा में भी उसे मानसिक शान्ति उपलब्ध नहीं हो सकती। शम, दम में कुशल योगी एकान्त गुहा में आनन्दपूर्वक शान्ति से रह सकता है। एक अनुरक्त पुरुष जिसने मन और इन्द्रियों का निग्रह नहीं किया, वह पर्वत-गुहा के एकान्त में भी हवाई किले बनायेगा।
पर्वत-गुहा में तो वही रह सकता है जो इच्छाओं से मुक्त है, संसार के प्रति आकृष्ट नहीं है, विवेकी है, मोक्ष की ज्वलन्त अभिलाषा रखता है और जिसने कई मास पर्यन्त मौन साधना की है।
गम्भीर, अनवरत ध्यान में प्रवेश करने से पूर्व योगासनों के नियमित अभ्यास से शरीर पर पूर्ण नियन्त्रण अनिवार्य है।
अपरिग्रह-किसी के धन की लालसा न करना, भौतिक वस्तुओं का संग्रह न करना।
आध्यात्मिक साधक को शारीरिक आवश्यकताओं की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। परमात्मा सब-कुछ देता है। प्रकृति ने पहले से ही सब प्रबन्ध कर रखे हैं। मनुष्य जितना अपना ध्यान रख सकता है, प्रकृति उससे कहीं अधिक कुशलता और सावधानी से उसकी देखभाल करती है। प्रकृति उसकी आवश्यकताओं को जानती है और वहीं उसी समय प्रदान करती है। माँ प्रकृति की रहस्यमयी प्रकृति को पहचानो और बुद्धिमान् बनो। उसकी अद्भुत दया, कृपा और करुणा के लिए उसके प्रति कृतज्ञ बनो।
यदि तुम ध्यानाभ्यास के लिए एकान्तवास चाहते हो और यदि तुम गृहस्थ हो कर भी घोर आध्यात्मिक साधना की पिपासा रखते हो, तो अनायास ही तुम अपने परिवार के साथ सम्बन्ध तोड़ नहीं सकते । सांसारिक सम्बन्धों का अनायास विच्छेद तुममें मानसिक अवसाद की स्थिति ला सकता है और परिवारी जन भी दुःखी होंगे। सम्बन्ध विच्छेद शनैः-शनैः करना उपयुक्त है। प्रारम्भ में सप्ताह अथवा माह पर्यन्त एकान्तवास करो। धीरे-धीरे समय की
अवधि बढ़ाते जाओ। तब वे वियोग की वेदना का अनुभव नहीं करेंगे। यदि तुम्हारी इच्छा-शक्ति दुर्बल है, तुम धार्मिक अनुशासन नहीं रख सकते अथवा युवावस्था में तुम्हें पाठशाला अथवा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण नहीं मिला और तुम भौतिकवाद में फंसे हुए हो, तो आवश्यक है कि कुछ दिनों अथवा सप्ताहों के लिए एकान्तवास को जाओ (क्रिसमस, ईस्टर अथवा अन्य छुट्टियों में) । वहाँ जा कर तुम कठोर तप और ध्यान-साधना करो और अपनी इच्छा-शक्ति बढ़ाओ ।
जिन्होंने अपने पुत्रों को नियुक्त कर लिया है और जो सेवा-निवृत्त हो गये हैं और गृहस्थ के कर्तव्यों से मुक्त हो चुके हैं, वे आत्म-शुद्धि और आत्म-सााक्षात्कार के लिए घोर तपस्या और ध्यान-साधना में लगने के लिए चार-पाँच वर्ष पर्यन्त एकान्तवास करें।
यह उच्चतर ज्ञान-प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय में पदार्पण (प्रवेश) करने के समान है। तपस् पूर्ण होने पर जब वे आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लें, तो बाहर आ कर वे प्रवचन, वाद-विवाद, संलाप (संकथा) अथवा आत्मा से आत्मा तक सन्देश पहुँचाना आदि अपनी सामर्थ्य और (ज्ञान पर) अधिकार के अनुसार ज्ञान का प्रसारण करें।
जहाँ कोई आकर्षण ही न हो, वहाँ इन्द्रियनिग्रह की परीक्षा कैसे करें? पर्याप्त प्रगति कर लेने पर समाज में लोगों के मध्य आ कर यौगिक साधक अपनी परीक्षा करे। किन्तु नित्य प्रति ऐसा न करे; क्योंकि जब कभी आत्म-निरीक्षण उस युवा की भाँति करने से, जो पौधे को नित्य जल से सींच कर उखाड़ कर देखता था कि पौधे की मूल गहरी गयी अथवा नहीं, हानि होगी।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ।।११ ।।
शब्दार्थ : शुचौ-पवित्र, देशे-स्थान में, प्रतिष्ठाप्यस्थापित कर के, स्थिरम् -स्थिरतापूर्वक, आसनम् आसन, आत्मनः-अपना, न नहीं, अत्युच्छ्रितम् - बहुत ऊँचा, न-नहीं, अतिनीचम् - बहुत नीचा, चैलाजिनकुशोत्तरम् -वस्त्र, मृगछाला और कुशासन एक के ऊपर एक रख कर ।
अनुवाद : पवित्र स्थान पर जो न अधिक ऊँचा हो न अधिक नीचा हो, आसन बिछा कर जो वस्त्र, मृगछाला और कुशा घास क्रमशः एक के ऊपर एक रख कर बना हो । (यहाँ पाठक्रम से वस्त्र आदि का क्रम उल्टा समझना चाहिए। पहले कुशा, फिर मृग-चर्म और अन्त में वस्त्र बिछाना चाहिए-शंकराचार्य)
व्याख्या : इस श्लोक में भगवान् ने ध्यानाभ्यास के लिए बाह्य आसन का निर्देश दिया है। मुद्राओं का विस्तार श्लोक १३ में है।
भूमि पर पहले कुशा बिछाओ, उस पर मृगछाला अथवा चीते की छाल और उसके ऊपर एक श्वेत वस्त्र बिछाओ।
प्राकृतिक पावन स्थान का चयन करो जैसे नदी का तट अथवा भूमि को स्वच्छ करो जहाँ भी तुम ध्यान करना चाहते हो।
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।
उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।।१२ ।।
शब्दार्थ : तत्र-वहाँ, एकाग्रम् एकाग्र, मन:-मन, कृत्वा कर के, यतचित्तेन्द्रियक्रियः - जिसने मन और इन्द्रियों की क्रियाओं को वश में कर लिया है, उपविश्य-बैठ कर, आसने-आसन पर, युञ्ज्यात्-अभ्यास करे, योगम्योग का, आत्मविशुद्धये-आत्म-शुद्धि के लिए।
अनुवाद : आसन पर बैठ कर, मन को एकाग्र कर के, चित्त और इन्द्रियों की प्रवृत्तियों को वश में कर के (साधक को) आत्म-शुद्धि के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।
व्याख्या : आत्मा का तात्पर्य यहाँ मन से है। वास्तविक परम तत्त्व तो आत्मा है। यह मुख्य है। मन भी आत्मा है; किन्तु यह गौण अर्थ में प्रयुक्त होता है। मुख्य आत्मन् ब्रह्म है, जब कि गौण आत्मा मन है।
योगाभ्यास के द्वारा मन की विकीर्ण वृत्तियों को संहृत करो। इन्द्रिय-विषयों से इसे पुनः-पुनः हटा कर अपने लक्ष्य, ध्यान-बिन्दु अथवा केन्द्र पर एकाग्रित करो । शनैः-शनैः मन एकाग्र होने लगेगा। अभ्यास नियमित होना अनिवार्य है। तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। नियमितता सर्वोच्च महत्त्व रखती है। आत्म-निरीक्षण अथवा दैनिक अन्तःपरीक्षण के द्वारा मन के रंग-ढंग जानने का प्रयास करो। मन के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, तब भटकते मन को नियन्त्रित करना सहज हो जायेगा। जब तुम ध्यान में बैठते हो और सांसारिक विषयों को स्वतः भुलाने का प्रयास करते हो, तो सब प्रकार के सांसारिक विचार तुम्हारे मन में विकसित होंगे और ध्यान में विघ्न डालेंगे। तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा। वर्षों पूर्व के विचार और सुखद स्मृतियाँ तुम्हारे मानस-पटल पर उभर कर आयेंगी और मन को इतस्ततः भ्रमण करने के लिए बाध्य करेंगी। तुम पाओगे कि विशाल अवचेतन मन का कूट द्वार (trap door) खुला है अथवा विचारों के कोष-गृह का आवरण हट गया है और विचार सतत अविरल धारा में बाहर प्रवाहित हो रहे हैं। जितना अधिक तुम उन पर नियन्त्रण पाने की कोशिश करते हो, उतनी अधिक द्विगुणित शक्ति से वह उभर कर आते हैं।
निरुत्साहित मत होओ। निराश मत होओ। निरन्तर नियमित अभ्यास से तुम अवचेतन मन की स्मृतियों को नष्ट कर सकते हो। ध्यानयोग की अग्नि सब विचारों को भस्म कर देगी। विश्वास रखो। विषयुक्त सांसारिक विचारों को नष्ट करने के लिए ध्यान प्रतिकारी औषध है। यह निश्चित है।
शाश्वत आत्मा पर ध्यान विस्फोटक की भाँति समस्त विचारों को और स्मृतियों को चेतन मन से उड़ा देगा। यदि विचार अधिक कष्ट पहुँचायें, तो 3/(3 - 6) बलपूर्वक दबाने का प्रयास न करो। चलचित्र के उपकरण की भाँति मौन साक्षी बने रहो। विचार स्वयं ही लुप्त हो जायेंगे। तत्पश्चात् नियमित मौन ध्यान से उन्हें समूल नष्ट करने का यत्न करो।
अन्तर्निरीक्षण के समय तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि मन कितनी शीघ्रता से दूसरी धारा में बदलता है। यहीं अवसर मिलता है मन को अपने अनुरूप संयत करने का। अब तुम विचार और मानसिक शक्ति को दिव्य स्रोत में उन्मुख कर सकते हो। अब विचारों का पुनः नवीनीकरण कर के सात्त्विक आधार पर नये विचारों की धारणा कर सकते हो। सांसारिक व्यर्थ विचारों को बाहर फेंक सकते हो। मन के दिव्य उद्यान में मोघ विचारों को तृणादि की भाँति बाहर कर के उत्कृष्ट, दिव्य विचारों के बीज डाल सकते हो। यह सहनशीलता का, धैर्य का कार्य है। वास्तव में यह अति-विशाल, विस्मयकारी कार्य है। किन्तु दृढ़प्रतिज्ञ योगी के लिए, जिस पर प्रभु की कृपा है और लौह समान इच्छा-शक्ति है, यह कुछ भी नहीं अर्थात् सहज है।
मूक ध्यान के द्वारा उभरते भावों, वृत्तियों, संवेगों और उत्तेजनाओं को धीरे-धीरे शान्त करो। सुव्यवस्थित सतत अभ्यास के द्वारा तुम अपने भावों को एक नवीन व उज्ज्वल दिशा प्रदान कर सकते हो। भौतिक प्रकृति को दिव्य प्रकृति में तन्मय कर सकते हो। ध्यान के द्वारा तुम स्नायु-तन्त्रों, मांसपेशियों, पंचकोषों, भावों, संवेगों और उत्तेजनाओं पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर सकते हो ।
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ।।१३ ।।
शब्दार्थ : समम् -सीधा, कायशिरोग्रीवम् - शरीर, सिर और गर्दन, धारयन् रखते हुए, अचलम्-अचल, स्थिरः-अचल, संप्रेक्ष्य-देखते हुए, नासिकाग्रम् नासिका के अग्रभाग को, स्वम्-अपने, दिशः-दिशाएँ, चऔर, अनवलोकयन् न देखते हुए।
अनुवाद : स्थिरतापूर्वक अपने शरीर, सिर और ग्रीवा को अचल और सीधा रखते हुए नासिकाग्र भाग पर दृष्टि एकाग्र कर के अन्य दिशाओं को न देखते हुए, कर रहे हैं, व्याख्या : इस श्लोक में भगवान् मुद्रा (आसन) और दृष्टि का वर्णन स्थिर आसन के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। यदि शरीर अस्थिर है, तो मन भी अस्थिर होगा। शरीर और मन का निकट का सम्बन्ध है।
शरीर को कदापि हिलाना नहीं चाहिए। नित्य अभ्यास के द्वारा आसन-जय प्राप्त करना चाहिए। चट्टान की भाँति सुदृढ़ रहो । शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा रखने से मेरुदण्ड सीधा रहेगा और कुण्डलिनी जागृत हो कर सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्व गमन करेगी। पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठो । इससे स्नायवीय सन्तुलन और मन की साम्यावस्था बनी रहेगी। स्थिरतापूर्वक दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखो। इसे 'नासिकाग्र दृष्टि' कहते हैं। अन्य दृष्टि हैं 'भूमध्य दृष्टि'-दोनों भौहों के मध्य आज्ञाचक्र पर दृष्टि टिकाना। इसका उल्लेख पाँचवें अध्याय के श्लोक २७ में हो चुका है। भ्रूमध्य दृष्टि में बन्द नेत्रों से आज्ञाचक्र पर दृष्टि एकाग्र की जाती है। खुली आँखों से करने पर सिर-दर्द हो सकता है। धूल अथवा विजातीय तत्त्व आँखों में गिर सकते हैं। मन भी भ्रमित हो सकता है। नेत्रों पर दबाव मत डालो। सहज अभ्यास करो। नासिकाग्र भाग पर ध्यान लगाने से दिव्य गन्ध की अनुभूति होती है। आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र करने से दिव्य ज्योति की अनुभूति होती है। यह एक अनुभूति है जो तुम्हें उत्साहित करने, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने और देहातीत अलौकिक संज्ञान के लिए तुम्हें बतायी गयी है। साधना बन्द मत करो। भगवान् शिव के भक्त और योगी जन आज्ञाचक्र पर भ्रूमध्य दृष्टि से मन एकाग्र करते हैं। कौन-सी दृष्टि तुम्हें अनुकूल पड़ती है, इसका चयन तुम कर सकते हो।
यद्यपि अर्ध खुले नेत्रों से दृष्टि नासिकाग्र भाग पर स्थिर की जाती है और नेत्र गोलक भी स्थिर रहते हैं। मन को आत्म-तत्त्व पर एकाग्र करना चाहिए। अतः तुम्हें मानो नासिकाग्र भाग पर ही देखना होगा। अध्याय VI. श्लोक 25 में भगवान् कहते हैं- “मन को आत्मा में स्थित कर के वह कोई और ध्यान न करे।" नासिकाग्र भाग पर दृष्टि स्थिर करने से मन अविलम्ब एकाग्रित होगा।
जिस भी बिन्दु का तुम चयन करो, वहीं अपने इष्टदेव के दर्शन करो और उसकी विद्यमानता की अनुभूति लो।
प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ।।१४।।
शब्दार्थ : प्रशान्तात्मा-शान्तचित्त, विगतभीः - निर्भय, ब्रह्मचारिव्रते- ब्रह्मचर्यव्रत में, स्थितः- दृढ़, मनः- मन, संयम्य-संयत कर के, मच्चित्तः- मेरा चिन्तन करते हुए, युक्त-समन्वित (सन्तुलित), आसीत-बैठे, मत्परः- मेरे परायण हो कर।
अनुवाद : शान्तचित्त, निर्भय, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़, जितेन्द्रिय पुरुष मेरा चिन्तन करता हुआ मुझे परम लक्ष्य मान कर (ध्यान में) बैठे।
व्याख्या : आध्यात्मिक साधक को शान्तचित्त रहना अत्यावश्यक है। दिव्य ज्योति शान्त चित्त में ही उतर सकती है। वासना, तृष्णा और इच्छा के दमन से चित्त की शान्ति अथवा मन की सौम्यता प्राप्त होती है। उसे निर्भय होना चाहिए। यह उत्कृष्ट गुण है। कायर व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार से बहुत दूर है (नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः) ।
ब्रह्मचारी को पूर्ण मन से गुरु की, आध्यात्मिक शिक्षक की सेवा करनी चाहिए और भिक्षा-वृत्ति पर निर्वाह करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। साधक को मन की वृत्तियों को संयत रखना चाहिए। सुख-दुःख, शीतोष्ण, मानापमान में समान रहना साधक के लिए हितकर है। भगवन्नाम का जप करते हुए साधक को सदा उसी को (भगवान् को) लक्ष्य मान कर आगे बढ़ना चाहिए।
ब्रह्मचर्य का अभिप्राय आत्म-नियन्त्रण अथवा इन्द्रिय-दमन भी है। वीर्य वह प्राण-शक्ति है जो नाड़ियों और मस्तिष्क को नियमित कर के प्रणाली को ऊर्जा प्रदान करती है। जिस ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा वीर्य-शक्ति की रक्षा की है और इसे ओज-शक्ति अथवा देदीप्यमान आध्यात्मिक शक्ति में परिणत कर दिया है, वह दीर्घावधि तक ध्यानाभ्यास में संलग्न रह सकता है। योग के सोपान पर वही आरोहण करने में सक्षम है। ब्रह्मचर्य-पालन अथवा आत्म-संयम के बिना किंचित् मात्र भी प्रगति सम्भव नहीं है। ब्रह्मचर्य की नींव पर ध्यान और समाधि के विशाल मन्दिर का निर्माण हो सकता है। बहुत लोग इस प्राण-शक्ति को व्यर्थ गँवाते हैं-जो वस्तुतः आध्यात्मिक सम्पदा है-किन्तु लोग सम्भोग की उत्तेजना में अन्धे हो कर ज्ञान-शक्ति को खो बैठते हैं। उनका भाग्य दयनीय है। वे योग में विशेष प्रगति नहीं कर सकते ।
युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः ।
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।। १५ ।।
शब्दार्थ : युञ्जन् -युक्त (समन्वित) रखते हुए, एवम् - इस प्रकार, सदा-सदा, आत्मानम् -स्वयं को, योगी-योगी, नियतमानसः- जिसने मन को वश में कर लिया है, शान्तिम्-शान्ति को, निर्वाणपरमाम् -मोक्ष प्रदायक, मत्संस्थाम् -मुझ में स्थित, अधिगच्छति -प्राप्त करता है।
अनुवाद : इस प्रकार मन को सदा सन्तुलित रखते हुए योगी जिसने अपने मन को संयत कर लिया है, उस निर्वाणपरक शान्ति को प्राप्त करता है जो मुझमें विद्यमान है।
व्याख्या : एवम् - इस प्रकार अर्थात् पूर्व श्लोक में निर्दिष्ट साधन के अनुरूप । परमात्मा शान्ति का मूर्तरूप (प्रतीक) है। वह शान्ति का सागर है। मन की वृत्तियों को नियन्त्रित कर के उन्हें सन्तुलित रखते हुए जो शाश्वत परमात्मा की परम शान्ति को प्राप्त करता है, वह निर्वाण को प्राप्त होता है।
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।। १६ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, अत्यश्नतः - अधिक खाने वाले का, तु-निश्चय से, योग: -योग, अस्ति -है , न-नहीं, च-और, एकान्तम् - नितान्त, अनश्नतःन खाने वाले का, ननहीं, च-और, अतिस्वप्नशीलस्य-अधिक सोने वाले का, जाग्रतः जागने वाले का, न-नहीं, एव-ही, च-और, अर्जुन-हे अर्जुन ।
अनुवाद : हे अर्जुन, योग न तो अधिक खाने वाले के लिए और न ही सर्वथा भोजन का त्याग करने वाले के लिए, न तो अधिक सोने वाले के लिए और न ही सर्वथा न सोने वाले के लिए सम्भव है।
व्याख्या : इस श्लोक में भगवान् यौगिक साधक के लिए भोजन का निर्देश कर रहे हैं। सोने और खाने में सदा युक्त रहना चाहिए। अधिक सोने से तुम तन्द्रिल (निद्रालु) बने रहोगे और निद्रा के वश में रहोगे। इससे अपच होगा, आँतों में वायु-विकार और यकृत के रोग विकसित होंगे। भोजन कम लेंगे, तो दुर्बलता के कारण ध्यान में दीर्घकाल तक बैठने में असमर्थ होंगे। शरीर की स्वस्थ और बलिष्ठ अवस्था में उसके निर्वाह के लिए जितना अनिवार्य है, उतना ही भोजन लेना चाहिए।
इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि योगशास्त्र में निर्दिष्ट भोजन के परिमाण से अधिक सेवन करने वाले के लिए योग में सफलता असम्भव है। ऐसा निर्देश है कि आधा पेट तो भोजन से भरा जाये, एक चौथाई पानी से और शेष चौथाई वायु की गति के लिए खाली रहे। योग के साधक के लिए यह मिताहार है।
अधिक सोने से तुम आलस्य, तन्द्रा में पड़े रहोगे। मन जड़ हो जायेगा और शरीर भारी। बहुत कम सोने पर भी तुम निद्रालु बने रहोगे। ध्यान में सोओगे । स्वर्णिम मध्यम मार्ग अपनाओ। योग में अविलम्ब सफलता मिलेगी।
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।।१७ ।।
शब्दार्थ : युक्ताहारविहारस्य-जिसका आहार-विहार युक्त (नियमित परिमाण में) है, युक्तचेष्टस्य कर्मसु कर्म करने में युक्त चेष्टा वाला, युक्तस्वप्नावबोधस्य-सोने और जागने में नियमित, योग:-योग, भवति होता है, दुःखहा-दुःख को नष्ट करने वाला।
अनुवाद : आहार-विहार कर्मों की चेष्टा तथा सुषुप्ति और जाग्रति में सम रहने वाले के लिए योग दुःखों को नष्ट करने वाला होता है।
व्याख्या : इस श्लोक में भगवान् योग के साधक को भोजन, आमोद-प्रमोद तथा विहार आदि का निर्देश देते हैं। योग के साधक को सदा सुखद मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। खाने-पीने में भगवान् बुद्ध अति कर गये थे। अत्यन्त मितभुज (अल्पाहारी) हो कर वे अत्यन्त दुर्बल हो गये। उन्होंने अपने शरीर को बहुत यातनाएँ दीं। इसीलिए वे योग में सफल न हो सके। आत्म-साक्षात्कार के लिए अत्यधिक तपस्या अनिवार्य नहीं है। अध्याय १७ के श्लोक ५ और ६ में भगवान् कृष्ण ने इसे गर्हित बताया है। आत्म-प्रताड़ना तपस्या नहीं है। यह तो पापिष्ठ है। भगवान् कृष्ण का बुद्धियोग तप के प्रति विवेकपूर्ण निर्देश है। कुछ साधक तो परित्याग को ही लक्ष्य मान लेते हैं। यह साधन है, लक्ष्य नहीं। स्नायु-मण्डल अत्यन्त संवेदनशील है। अत्यल्प परिवर्तन का भी यह सन्देश देता है जिससे मन भ्रमित होता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि जीवन नियमित हो, अनुशासित हो; आहार, निद्रा और आमोद-प्रमोद में सन्तुलित हो । मिताहारी बनो। निर्दिष्ट समय पर शयन और जागरण करो। ९ बजे अथवा १० बजे तक सो जाओ और ३ अथवा ४ बजे शय्या त्याग दो । तभी योग में सफलता सम्भव है जो इस जीवन के समस्त दुःखों से, क्लेशों से मुक्त कर देगा।
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।।१८ ।।
शब्दार्थ : यदा-जब, विनियतम् - पूर्णरूपेण वशीभूत, चित्तम् -मन, आत्मनि-आत्मा में, एव-ही, अवतिष्ठते-विश्राम करता है, निःस्पृहः-कामना रहित, सर्वकामेभ्यः समस्त इच्छाओं (विषयों) से, युक्तः समन्वित, इति-इस प्रकार, उच्यते-कहा जाता है, तदा-तब ।
अनुवाद : समस्त कमनीय पदार्थों की इच्छा से मुक्त और पूर्ण रूप से नियन्त्रित मन जब आत्मा में स्थित होता है, तब वह युक्त (योग में लीन) ऐसा कहा जाता है।
व्याख्या : विनियतम् -पूर्ण एकाग्रता के साथ ।
दृश्य-अदृश्य सब प्रकार के इच्छित पदार्थों की लालसा जब मर जाती है, तो मन प्रशान्त हो कर स्थिरतापूर्वक आभ्यन्तर आत्मा में स्थित हो जाता है। क्योंकि योगी पूर्णरूपेण समन्वय की स्थिति में होता है, उसने आत्मा के साथ समस्वरता प्राप्त कर ली है और ऐक्यभाव में आ गया है, तो शरीर की आसक्ति और इन्द्रियों का प्रपंच (दृश्य जगत्) उसे भ्रमित नहीं करते। वह अपनी अमृतमयी, अनश्वर और अजय्य प्रकृति के प्रति चैतन्य होता है।
युक्त का अभिप्राय है समस्वर (आत्मा के साथ), समन्वित, सन्तुलित । आत्मैक्य के बिना न तो समन्वय, न सन्तुलन और न ही समाधि सम्भव है। (निरूपण-V.23; V1.8)
यथा दीपो निवातस्थी नेङ्गते सोपमा स्मृता ।
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ।।१९ ।।
शब्दार्थ : यथा-जिस प्रकार, दीप:-दीपक, निवातस्थः वातरहित स्थान में रखा हुआ, ननहीं, इङ्गते-हिलता, सा-वही, उपमा-उपमा (तुलना), स्मृता-मानी गयी है, योगिनः योगी की, यतचित्तस्य-संयत चित्त वाले की, युञ्जतः-अभ्यासरत, योगम्-योग, आत्मनः- आत्मा का।
अनुवाद : आत्मा के साथ संयोग करने का अभ्यास करने वाले जितेन्द्रिय योगी की उपमा उस दीपक से की जाती है जो वायु रहित स्थान में स्थित होने के कारण लोलित (चलायमान) नहीं होता ।
व्याख्या : यह एक सुन्दर उपमा है। मन की एकाग्रता, स्थिरता और समस्वरता का वर्णन करते समय प्रायः इस उपमा का संकेत देते हैं। सुस्थिर मन वह शक्तिशाली प्रकाशदीप है जो आत्मा के गुप्त आध्यात्मिक कोष को खोजने में समर्थ है, सक्षम है।
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।।२० ।।
शब्दार्थ : यत्र-जहाँ, उपरमते-शान्त हो जाता है, चित्तम् -चित्त, निरुद्धम् - वश में किया हुआ, योगसेवया-योगाभ्यास के द्वारा, यत्र-जहाँ, च-और, एव-ही, आत्मना-आत्मा से, आत्मानम् - आत्मा पश्यन् देखता हुआ, आत्मनि-आत्मा में, तुष्यति-सन्तुष्ट होता है। को,
अनुवाद : योग के अभ्यास से उपराम हुआ चित्त जब आत्मा से आत्मा को देखता हुआ निज आत्मा में सन्तुष्ट हो जाता है,
व्याख्या : श्लोक २०, २१, २२ और २३ एक-साथ लेने चाहिए। विषयों से पूर्णतया परावर्तित मन ही परम शान्ति का साम्राज्य प्राप्त करता है। एकाग्रता के अनवरत और दृढ़ अभ्यास से जब मन स्थिर हो जाता है, तब योगी मन के द्वारा इस परमात्मा के दर्शन करता है; क्योंकि अब मन परिमार्जित तथा एकाग्र हो चुका है और आभ्यन्तर में परम शान्ति का अनुभव करता है।
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।।२१ ।।
शब्दार्थ : सुखम् -सुख, आत्यन्तिकम् - अनन्त, यत्-जो, तत् वह, बुद्धिग्राह्यम् बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य, अतीन्द्रियम् - इन्द्रियों से अतीत (परे), वेत्ति जानता है, यत्र-जहाँ, ननहीं, च-और, एव-ही, अयम्-यह, स्थितः-स्थित, चलति-चलता है, तत्त्वतः सत्य से।
अनुवाद : इन्द्रियों से अतीत सूक्ष्म परिमार्जित बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनन्त आनन्द की अनुभूति जब योगी को होती है और वह उस स्थिति को प्राप्त कर के जब सत्य से कभी विचलित नहीं होता,
व्याख्या : आत्मा का असीम आनन्द (जो इन्द्रियों की पहुँच से परे है) स्वतन्त्र रूप से केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ही साक्षात्कार किया जा सकता है। गहन ध्यान की अवस्था में इन्द्रियाँ अपने कारणस्वरूप मन में लीन होने के कारण निष्क्रिय हो जाती हैं। बुद्धि पवित्र होती है यम, नियम और सतत ध्यान से।
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।।२२ ।।
शब्दार्थ : यम् -जिसको, लब्ध्वा-प्राप्त कर, च-और, अपरम् अन्य, लाभम् - लाभ, मन्यते मानता है, न-नहीं, अधिकम् - (इससे) बढ़ कर, ततः-उससे, यस्मिन् -जिसमें, स्थितः - स्थित, न-नहीं, दुःखेन दुःख से, गुरुणा-कठिन होने पर, अपि-भी, विचाल्यते-विचलित होता है।
अनुवाद : जिसे प्राप्त कर लेने पर वह सोचता है, इससे बढ़ कर और कोई लाभ श्रेष्ठतर नहीं है और जिस अवस्था में स्थित हो कर वह बड़े-से-बड़े दुःख में भी विचलित नहीं होता।
व्याख्या : यम् - लाभ, आत्म-साक्षात्कार अथवा शाश्वत आत्मा के सन्दर्भ में प्रयुक्त है।
यस्मिन्-आनन्दस्वरूप आत्मा जो भ्रम और दुःख से अतीत है। आत्मा सम्पूर्ण रूप है और स्वयं में स्थित है। इसे प्राप्त कर सर्व कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस कारण भगवान् कहते हैं-"इससे बढ़ कर प्राप्तव्य कोई और लाभ नहीं है। आत्म-साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च लाभ है।" यदि कोई अपने भीतर स्थित इस आत्म-तत्त्व में स्थित हो जाता है, संसार के कोई दुःख उसे चलायमान नहीं कर सकते; क्योंकि दुःख की अनुभूति करने वाले मन से वह अब अतीत हो चुका है। उसने ब्रह्मैक्य स्थापित कर लिया है। मन और शरीर के साथ एकत्व भाव होने पर दुःख की अनुभूति होती है। मन नहीं, तो दुःख नहीं। हाथ कटने पर भी, क्लोरोफार्म के नशे में मनुष्य दुःख-पीड़ा का अनुभव नहीं करता; क्योंकि मन को शरीर से परावृत कर दिया गया है।
तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।। २३ ।।
शब्दार्थ : तम् - उसे, विद्यात्-जाने, दुःखसंयोगवियोगम् दुःख के साथ संयोग की अवस्था से वियोग, योगसंज्ञितम्-जिसे योग की संज्ञा दी गयी है, सः- वह, निश्चयेन-निःसन्देह, योक्तव्यः - अभ्यास किया जाना चाहिए, योग:- योग, अनिर्विण्णचेतसा -उत्साहित (आशापूर्ण) मन से ।
अनुवाद : दुःख के साथ संयोग का वियोग ही योग अभिहित है। दृढ़संकल्प (निश्चय) और अनुद्विग्न (उत्साहित) मन से योग का अभ्यास किया जाना चाहिए।
व्याख्या : श्लोक २०, २१ और २२ में भगवान् योग के लाभ से अवगत कराते हैं अर्थात् आत्मस्थ हो कर पूर्ण तुष्टि प्राप्त करना, अनन्त-असीम आनन्द, दुःखों से मुक्ति आदि। आगे वे उपदेश देते हैं कि यह योग दृढ़संकल्प, लौह-निश्चय तथा अनवसाद की अवस्था में किया जाना चाहिए। चंचल वृत्ति से युक्त आध्यात्मिक साधक योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। मार्ग की बाधाओं से निराश हो कर वह अभ्यास छोड़ देगा। अभ्यासी को प्रसन्नचित्त, बलवान् और आत्म-संयमी होना चाहिए।
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।।२४ ।।
शब्दार्थ : संकल्पप्रभवान् -संकल्प से उद्भूत, कामान् - इच्छाओं को, त्यक्त्वा-त्याग कर, सर्वान् -सब, अशेषतः - निःशेष रूप से, मनसा-मन के द्वारा, एव-ही, इन्द्रियग्रामम् - इन्द्रियों के समूह को, विनियम्य-संयत करके, समन्ततः सब ओर से ।
अनुवाद : संकल्प से उद्भूत समस्त इच्छाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा सब ओर से इन्द्रिय-समूह को पूर्णतया वशीभूत कर के,
व्याख्या : अशेषतः मन एक चतुर नीतिज्ञ है, अपनी सन्तुष्टि के लिए कतिपय इच्छाएँ वह गुप्त रूप से रखता है। अतः समस्त इच्छाओं का त्याग पूर्ण रूप से ही करना चाहिए। कोई इच्छा शेष नहीं रखनी चाहिए।
इच्छा का उद्भव संकल्प से है; अतः पहले तो संकल्प को नष्ट करो। यदि संकल्प का लोप हो जाये, तो इच्छा स्वतः ही लुप्त हो जायेगी। ध्यान रहे, मन के द्वारा सब ओर से सभी इच्छाओं का त्याग और इन्द्रियनिग्रह होना चाहिए। यदि एक भी इन्द्रिय किसी दिशा-विशेष में व्याकुल है, तो मन को प्रायः विह्वल (क्षुब्ध) करेगी। प्रत्याहार के निरन्तर अभ्यास से इन्द्रियाँ मन में विलीन हो जायेंगी। तब मन किसी तन्मात्रा का चिन्तन नहीं करेगा और पूर्ण शान्ति को प्राप्त करेगा।
प्रबल विवेक-शक्ति और अनासक्ति से युक्त मन इन्द्रिय-समूह को सब दिशाओं से उनके विषयों से पराङ्मुख करने में सक्षम होगा। अतः प्रबल विवेक का विकास करो-नित्य-अनित्य का भेद करने के लिए और विषय-वासनाओं से पूर्णरूपेण विरक्त होने के लिए। (निरूपण -11.62)
शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धया धृतिगृहीतया ।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।। २५ ।।
शब्दार्थ : शनैः शनैः- धीरे-धीरे, उपरमेत् -निवृत्त रहे, उपरति को प्राप्त करे, बुद्धया-बुद्धि से, धृतिगृहीतया-विश्वासपूर्वक, आत्मसंस्थम् - आत्मा में स्थित (समाधि में स्थित), मनः-मन, कृत्वा कर के, न-नहीं, किञ्चित् -कुछ भी, अपि-भी, चिन्तयेत् सोचे।
अनुवाद : धीरे-धीरे स्थिरतापूर्वक विश्वास के साथ बुद्धि को नियन्त्रित करके, मन को प्रशान्त कर के आत्मा में स्थित कर के अन्य कोई चिन्तन न करे।
व्याख्या : दृढ़ संकल्प से बुद्धि को अनुगृहीत करके योगाभ्यासी क्रमशः प्रशान्तता को प्राप्त करे। स्थिर एकाग्रता का सतत दीर्घ अभ्यास हृदय को क्रमशः परमात्मा की अनिर्वचनीय शान्ति से और आनन्द से पुलकित (रोमांचित) कर देगा। योगाभ्यासी को चाहिए कि वह सतत अभ्यास के द्वारा मन को निरन्तर आत्मा में स्थित करे। अमर आत्मन्, परमात्मन् का सतत चिन्तन मन को उसके ऐन्द्रिक विषय-सुख से विमुख कर देगा । आत्म-चिन्तन के द्वारा मानसिक शक्ति को आध्यात्मिक स्रोत की ओर उन्मुख करें।
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ।।२६ ।।
शब्दार्थ : यतः यतः-जिस-जिस निमित्त से, निश्चरति-विचरता है, मनः-मन, चञ्चलम् चञ्चल, अस्थिरम्-अस्थिर, ततः ततः-उस-उस से, नियम्य-संयत कर के, एतत् यह, आत्मनि-आत्मा में, एव-ही, वशम् वश में, नयेत् लावे।
अनुवाद : जिस-जिस निमित्त से यह चञ्चल और अस्थिर मन इतस्ततः भटकता है, उसी से हटा कर, वश में कर के (साधक) आत्मा में स्थित करे ।
व्याख्या : इस श्लोक में भगवान् मन को नियन्त्रित करने का उपाय बताते हैं। वृषभ के भागने पर जैसे तुम पुनः पुनः उसे घर की ओर खींचते हो, उसी प्रकार से बाह्य विषयों में विचरण करने वाले मन को पुनः-पुनः अपने लक्ष्य, केन्द्र में स्थापित करो । यदि तुम उसे बिनौले, गुड़, केला आदि दोगे, तो वह घर में ही रहेगा, बाहर नहीं भागेगा। इसी प्रकार से यदि तुम मन को आन्तरिक शाश्वत आनन्द का स्वाद शनैः-शनैः योगाभ्यास के द्वारा चखा दोगे तो यह बाह्य इन्द्रिय-विषयों में भटकना बन्द कर देगा। शब्दादि विषय मन को व्याकुल और अस्थिर करते हैं। ऐन्द्रिक सुखों के दोषों को जान कर, उनकी भ्रमित करने वाली प्रकृति को समझ कर तुम मन को पूर्णतया विषयों से हटा कर दृढ़तापूर्वक आत्म-संस्थित कर सकते हो, परन्तु इसके लिए तुम्हें नित्यानित्य-वस्तु-विवेक करना होगा, अनासक्ति का विकास करना होगा और मन को आत्मा के गौरव और विशिष्टतम तेजस् से अवगत कराना होगा।
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ।। २७ ।।
शब्दार्थ : प्रशान्तमनसम् - शान्त-चित्त वाला, हि-निश्चित रूप से, एनम् -ऐसे, योगिनम् - योगी को, सुखम् -आनन्द, उत्तमम् उत्तम, उपैति प्राप्त होता है, शान्तरजसम्-जिसकी आसक्ति शान्त हो गयी है, ब्रह्मभूतम् ब्रह्म के साथ एक रूप होने वाला, अकल्मषम् - पाप रहित ।
अनुवाद : उस योगी को परमानन्द (उत्तम सुख) की प्राप्ति होती है जिसका मन प्रशान्त है, जिसका रजोगुण शान्त हो गया है और जिसने पापों से मुक्त हो कर ब्रह्मैक्य स्थापित कर लिया है।
व्याख्या : इस श्लोक में तथा अगले श्लोक में भगवान् योग के लाभ का वर्णन करते हैं।
नित्य, शुद्ध, अबाधित अनन्त आनन्द की अनुभूति उस योगी को होती है जिसका मन पूर्ण रूप से शान्त है, सौम्य है, जिसने अपनी रजोगुणी प्रवृत्ति को शान्त कर लिया है, जिसने सब प्रकार की आसक्तियों को नष्ट कर दिया है, जो आत्म-ज्ञान प्राप्त कर के जीवन्मुक्त हो गया है, जो सब प्राणियों में ब्रह्मभाव रखता है और जो निष्कलंक है अर्थात् अच्छे-बुरे और धर्म-अधर्म से प्रभावित नहीं होता।
युज्ञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः ।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ।।२८ ।।
शब्दार्थ : वुञ्जन् योगाभ्यास करते हुए, एवम् - इस प्रकार, सदा-सदा, आत्मानम् - आत्मा का, मन का, योगी-योगी, विगतकल्मषः-पाप से मुक्त, सुखेन-सुख से, ब्रह्मसंस्पर्शम् - ब्रह्म के सान्निध्य (संस्पर्श) में होने वाले, अत्यन्तम् अनन्त, सुखम् -सुख को, अश्नुते-प्राप्त करता है।
अनुवाद : इस प्रकार पाप-मुक्त हो कर योगाभ्यास में मन को नियुक्त करता हुआ योगी सहज रूप से ब्रह्म-संस्पर्श के अनन्त आनन्द की अनुभूति करता है।
व्याख्या : प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि योग के अभ्यास से योगी विषयों से हट कर नित्य शाश्वत ब्रह्म के सम्पर्क में आ जाता है और ब्रह्मानन्द को प्राप्त होता है।
विषय-सुख क्षण-भङ्गुर है, अनित्य है; किन्तु ब्रह्मानन्द अबाधित, अक्षय्य और नित्य है। इसी कारण से अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए उसे आभ्यन्तर में प्राप्त करने का।
योगी मार्ग में आने वाली सब बाधाओं को दूर करता हुआ परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करता है और मन को आत्मा में ही स्थिर रखता है।
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।।२९ ।।
शब्दार्थ : सर्वभूतस्थम् -सब प्राणियों में विद्यमान, आत्मानम् स्वयं को, सर्वभूतानि-सब प्राणियों को, च-और, आत्मनि-आत्मा में, ईक्षते-देखता है, योगयुक्तात्मा-योग से युक्त (समन्वित) हुआ पुरुष, सर्वत्र सब जगह, समदर्शनः समदृष्टि ।
अनुवाद : योग द्वारा समस्वरता प्राप्त कर लेने पर योगी सब प्राणियों में (निज) आत्मा को और (निज) आत्मा में सब प्राणियों को स्थित देखता है। वह सर्वत्र उसी आत्म-तत्त्व के दर्शन करता है।
व्याख्या : ज्ञान-चक्षु अथवा दिव्य दृष्टि द्वारा योगी सर्वत्र आत्मा की एकता का अनुभव करता है। वस्तुतः यह दृष्टि उत्कृष्ट और उदारचेतसा है। वह सर्वत्र ब्रह्मानुभूति करता है। वह देखता है कि जगत् ब्रह्ममय है और जीवात्मा ब्रह्मस्वरूप है।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।। ३० ।।
शब्दार्थ : यः-जो, माम् -मुझे, पश्यति-देखता है, सर्वत्र-सब जगह, सर्वम् सब-कुछ, च-और, मयि-मुझमें, पश्यति-देखता है, तस्य-उसके लिए, अहम् -मैं, ननहीं, प्रणश्यामि-अदृश्य होता हूँ, सः- वह, च-और, मे-मेरे लिए, न-नहीं, प्रणश्यति- अदृश्य होता है।
अनुवाद : जो पुरुष मुझे सर्वत्र देखता है और सर्वस्व मुझमें देखता है, वह कभी मुझसे दूर नहीं होता और न ही मैं उसके लिए अदृश्य होता हूँ।
व्याख्या : इस श्लोक में भगवान् दिव्य दृष्टि के प्रभाव का निरूपण कर रहे हैं।
जो सब प्राणियों में मुझे ही आत्म-रूप से देखता है और सर्वस्व, ब्रह्मा से ले कर तृण पर्यन्त मुझमें देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं और योगी दोनों आत्म-रूप से एक हो जाते हैं। न तो वह मेरी विद्यमानता के अभाव का अनुभव करता है और न ही मैं उसकी विद्यमानता का अभाव होने देता हूँ। वह मुझमें व्याप्त रहता है और मैं उसमें व्याप्त रहता हूँ।
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।। ३१ ।।
शब्दार्थ : सर्वभूतस्थितम् -सब प्राणियों में स्थित, यः-जो, माम् मुझे, भजति-भजता है, एकत्वम् -एकत्व, आस्थितः-स्थित, सर्वथा-सब प्रकार से, वर्तमानः रहते हुए, अपि भी, सः-वह, योगी-योगी, मयि मुझमें, वर्तते-रहता है।
अनुवाद : अभेद रूप में स्थित जो पुरुष मुझे सब प्राणियों में स्थित मान कर मेरा भजन करता है, वह योगी संसार में चाहे कैसे भी क्रियाशील रहे (आन्तरिक रूप से) मुझमें निवास करता है।
व्याख्या : आत्मस्थ-एकीभाव में जिसका द्वैत लुप्त हो गया है, जो एकत्व में स्थित है, मेरी उपासना करता है अर्थात् जिसने सब प्राणियों की अन्तरात्मा के रूप में मेरा साक्षात्कार कर लिया है, सदा मुझमें निवास करता है, उसके जीवन का ढंग कुछ भी हो, वह सदा मुक्त है।
कसाई होते हुए भी सदना का मन सदा भगवान् के चरण-कमलों में स्थित रहता था।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।। ३२ ।।
शब्दार्थ : आत्मौपम्येन-आत्मा की सादृश्यता से, सर्वत्र सब जगह, समम् -समान, पश्यति-देखता है, यः-जो, अर्जुन-हे अर्जुन, सुखम् -सुख, वा-और,यदि-यदि , वा-अथवा, दुःखम्-दुःख, सः- वह, योगी-योगी, परमः परम, मतः माना जाता है।
अनुवाद : हे अर्जुन, जो पुरुष आत्मवत् सर्वत्र समदृष्टि रखता है, दुःख हो अथवा सुख, सदा सम रहता है, वह परम योगी कहलाता है।
व्याख्या : अन्य लोगों में और मुझमें सुख-दुःख की अनुभूति वह समान रूप से करता है। वह किसी को हानि नहीं पहुँचाता। वह सर्वथा हानि रहित है। वह सबके कल्याण की कामना करता है। सभी प्राणियों के प्रति वह दयार्द्र है। उसका हृदय विशाल और कोमल होता है। आत्मा में स्थित हो कर वह सर्वत्र आत्म-दर्शन करता है; क्योंकि उसने सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अतः वह समस्त योगियों में सर्वोत्कृष्ट योगी मन्तव्य है।
अर्जुन उवाच
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् ।। ३३ ।।
शब्दार्थ : यः-जो, अयम् - यह, योगः- योग, त्वया- आपके द्वारा, प्रोक्तः-बताया गया, साम्येन-समता के द्वारा, मधुसूदन- हे मधुसूदन (कृष्ण), एतस्य-इसकी, अहम् -मैं, न नहीं, पश्यामि-देखता हूँ, चञ्चलत्वात्- चञ्चलतावश, स्थितिम् - स्थिति, स्थिराम् - स्थिर ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे कृष्ण, मन की चञ्चलता के कारण आपके द्वारा उपदिष्ट इस समतायोग की स्थिरता को मैं नहीं देख रहा।
व्याख्या : मन की अस्थिरता, व्याकुलता और तीव्र संवेग के कारण आपके द्वारा बताये गये समयोग का अभ्यास दुष्कर-सा प्रतीत हो रहा है। भगवन्, पलक झपकते ही मन इधर-उधर भटकता है, इसी कारण मैं स्थिरतापूर्वक मन को एकाग्र करने में असमर्थ हूँ।
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।।३४ ।।
शब्दार्थ : चञ्चलम् - अस्थिर, हि-निस्सन्देह, मनः मन, कृष्ण-हे कृष्ण, प्रमाथि उच्छृंखल, बलवत्-बलवान्, दृढम् -हठी, तस्य-उसका, अहम् -मैं, निग्रहम् -वशीकरण, मन्ये—मानता हूँ, वायो:-वायु की, इव-भाँति, सुदुष्करम् करने में कठिन।
अनुवाद : निश्चित रूप से मन चञ्चल, उच्छृंखल, बलवान् और हठीला है। हे कृष्ण, इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान कठिन है।
व्याख्या: मन के विषय परिवर्तित होते रहते हैं; अतः यह सदा व्याकुल रहता है।
'कृष्ण' शब्द कृष् धातु से बना है जिसका अभिप्राय है-खींचना, आकृष्ट करना । कृष्ण अपने भक्तों के हृदयों के समस्त पाप, अशुभ कर्म और बुराई के मूल को दूर कर देते हैं; इसीलिए वे कृष्ण हैं।
मन केवल चञ्चल ही नहीं है, वह उच्छृंखल, बलवान् और हठी भी है। इन्द्रियों और शरीर में यह हिंसात्मक उत्तेजना उत्पन्न करता है। सभी दिशाओं से विषयों में इसका आकर्षण है। पाँच इन्द्रियों के सहयोग से यह कार्य करता है। इनके द्वारा वह पाँच प्रकार के विषयों की ओर आकृष्ट होता है। इसीलिए यह सदा व्याकुल रहता है। शरीर और इन्द्रियों के सहयोग से यह इन पाँच प्रकार के विषयों का सुख-भोग करता है। इसीलिए इन्द्रियाँ बाह्य विषयों में प्रवृत्त होती हैं और प्रभावित होती हैं। इसे वश में करना तो वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। मन वायु तन्मात्रा से उत्पन्न है; इसी कारण यह वायु की भाँति अस्थिर है।
श्री भगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।। ३५ ।।
शब्दार्थ : असंशयम् - निस्सन्देह, महाबाहो - 3 महाबाहो अर्जुन, मनः-मन, दुर्निग्रहम् दमन करना कठिन, चलम् - चलायमान (अशान्त), अभ्यासेन अभ्यास के द्वारा, तु-किन्तु, कौन्तेय-हे कुन्तिपुत्र, वैराग्येण - वैराग्य द्वारा, च -और, गृह्यते वश में किया जाता है।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : हे महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई सन्देह नहीं कि मन को नियन्त्रित करना दुष्कर है और मन अस्थिर है, तदापि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है।
व्याख्या : चञ्चल मन को स्थिर करने के लिए लक्ष्य पर सतत ध्यान का अनवरत अथवा पुनः पुनः प्रयास ही अभ्यास है। आत्मा अथवा परमात्मा के उसी विचार की पुनरावृत्ति की जाती है। यह सतत पुनरावृत्ति मन के विक्षेप और कामनाओं का विनाश कर के उसे स्थिरता की ओर उन्मुख करती है।
इहलोक में अथवा परलोक में, यहाँ अथवा वहाँ, दृश्य अथवा अदृश्य, श्रुत अथवा अश्रुत ऐन्द्रिक-विषयों में दोष-दृष्टि प्राप्त होने पर उन विषयों के प्रति विरक्ति (अनासक्ति) वैराग्य है। सच्चिदानन्दस्वरूप शाश्वत आत्मा पर निरन्तर ध्यान द्वारा मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। सांसारिक विषयों की क्षणभंगुरता की प्रकृति से मन को अवगत कराना अनिवार्य है। मन को समझाना चाहिए कि नश्वर, परिवर्तनशील, बाह्य विषयों से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । सुख तो अन्तर्निहित कूटस्थ अमर आत्मा में है। शनैः-शनैः मन बाह्य विषयों से दूर हो जायेगा।
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवामुमुपायतः ।। ३६ ।।
शब्दार्थ : असंयतात्मना अनियन्त्रित मन वाले के द्वारा, योगः योग, दुष्प्रापः- प्राप्त करना कठिन, इति-इस प्रकार, मे—मेरा, मतिः-विचार, वश्यात्मना संयत पुरुष के लिए, तु-किन्तु, यतता-प्रयत्न करते हुए, शक्य:- सम्भव, अवाप्तुम् - प्राप्त करने के लिए, उपायतः - उपयुक्त साधन द्वारा ।
अनुवाद : असंयत व्यक्ति के लिए योग दुष्प्राय है; किन्तु संयत और यत्नशील इसे उपयुक्त साधन द्वारा प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मत है।
व्याख्या : असंयत आत्मा-जिसने ध्यान और विरक्ति के सतत अभ्यास से इन्द्रियों और मन को वश में नहीं किया।
संयत आत्मा-जिसने वैराग्य और ध्यान के अभ्यास से मन को वशीभूत कर लिया है। ऐसा मनुष्य उपयुक्त साधन और सतत प्रयास के द्वारा आत्म-साक्षात्कार कर सकता है।
अर्जुन उवाच
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ।
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ।। ३७ ।।
शब्दार्थ : अयतिः-असंयमी, श्रद्धया-श्रद्धा से, उपेतः युक्त, योगात् योग से, चलितमानसः-विचलित मन वाला, अप्राप्य-प्राप्त न कर के, योगसंसिद्धिम् योग में पूर्णता, काम् -कौन-सी, गतिम् - गति को, कृष्ण-हे कृष्ण, गच्छति-प्राप्त करता है।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे कृष्ण, श्रद्धावान् होते हुए भी स्वयं को संयत करने में असमर्थ व्यक्ति जिसका मन योग से विचलित हो चुका है, योग में सिद्धि प्राप्त करने में असफल होने पर कौन-सी गति (दशा) को प्राप्त होता है?
व्याख्या : उसे योग की अमोघता अथवा प्रभाव में पूर्ण विश्वास है, किन्तु वह इन्द्रियों और मन को वश में करने में समर्थ नहीं है। उसका मन एकाग्रचित्त नहीं है। शरीर में अन्तिम श्वास के समय उसका मन भटक जाता है और वह अपनी स्मृति खो बैठता है। योग में निपुणता अर्थात् आत्म-साक्षात्कार अथवा आत्म-ज्ञान प्राप्त करने में असफल वह व्यक्ति किस मार्ग पर जायेगा, उसकी अन्तिम दशा क्या होगी?
कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।। ३८ ।।
शब्दार्थ : कच्चित् -क्या ऐसा है?, ननहीं, उभयविभ्रष्टः दोनों से पतित, छिन्नाभ्रम् -फटे हुए (छिन्न-भिन्न) बादल, इव-समान, नश्यति-नष्ट हो जाता है, अप्रतिष्ठः- आश्रय रहित, महाबाहो - हे बलिष्ठ बाहो (कृष्ण), विमूढः - भ्रमित, ब्रह्मणः -ब्रह्म के, पथि-पथ में।
अनुवाद : हे महाबाहो (कृष्ण), दोनों ओर से पतित, आश्रय रहित हो कर ब्रह्म के मार्ग में भ्रमित (किंकर्तव्यविमूढ़) हो कर छिन्न-भिन्न बादल की भाँति नष्ट तो नहीं हो जाता?
व्याख्या : उभय-कर्म-मार्ग अथवा वेदविहित कर्मकाण्ड के अनुरूप यज्ञादि अनुष्ठान एक ओर तथा ज्ञानयोग का मार्ग दूसरी ओर ।
ब्रह्मणः पथि-वह पथ जिसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है।
भगवान् द्वारा उपदिष्ट योग यहाँ अभ्यास में पूर्ण निष्ठा की अपेक्षा करता है। साधक संसार से भी दूर और स्वर्ग से भी दूर चला जाता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि साधक यदि लक्ष्य प्राप्ति tilde pi सफल न हुआ, तो बिना बात के वह सर्वस्व खो देगा। इसी सन्दर्भ में अगला प्रश्न है।
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः ।
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।। ३९ ।।
शब्दार्थ : एतत् यह, मे-मेरे, संशयम् -सन्देह को, कृष्ण-हे कृष्ण, छेत्तुम् दूर करने में, अर्हसि समर्थ हो, अशेषतः- पूर्ण रूप से, त्वत् तुमसे, अन्यः-अन्य, संशयस्य-संशय का, अस्य-इस, छेत्ता-दूर करने वाला, ननहीं, हि-निश्चित रूपेण, उपपद्यते योग्य (समर्थ) है।
अनुवाद : हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से दूर कर दें; क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को नष्ट करने में सक्षम नहीं है।
व्याख्या : आपके सिवा अन्य कोई प्रशस्ततर शिक्षक नहीं हो सकता; क्योंकि आप तो सर्वज्ञ भगवान् हैं। आप ही इस संशय का निवारण कर सकते हैं। कोई ऋषि, देव अथवा मुनि इस संशय को नष्ट नहीं कर सकते।
श्री भगवानुवाच
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
नहि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गतिं तात गच्छति ।।४० ।।
शब्दार्थ : पार्थ-पार्थ (अर्जुन), न-नहीं, एव-ही, इह -यहॉं, न -नहीं , अमुत्र-परलोक में, विनाशः - विनाश, तस्य-उसका, विद्यते- (होता) है, न-नहीं, हि-निश्चित रूप से, कल्याणकृत् -कल्याण करने वाला, कश्चित्-कोई, दुर्गतिम् बुरी दशा को, तात- हे पुत्र (प्रिय), गच्छति-प्राप्त होता है।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : हे अर्जुन, न तो इस लोक में न ही परलोक में उसका विनाश सम्भव है। प्रिय पुत्र, अच्छे कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्दशा को प्राप्त नहीं होता।
व्याख्या : इस जन्म में जो साधक योग में सफल नहीं हो सका, वह न तो इस लोक में और न ही दूसरे लोक में विनाश को प्राप्त होगा। निश्चित रूप से वह निम्न योनि में जन्म नहीं लेगा। फिर वह क्या प्राप्त करेगा? इसका वर्णन भगवान् श्लोक ४१, ४२, ४३ और ४४ में करते हैं।
तात-शिष्य पुत्र समान होता है।
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ।।४१ ।।
शब्दार्थ : प्राप्य-प्राप्त कर के, पुण्यकृताम् - पुण्य कर्म करने वालों के, लोकान् लोकों को, उषित्वा-वास कर के, शाश्वतीः- अनेक, समाः वर्ष, शुचीनाम् - पवित्रात्माओं के, श्रीमताम् -सम्पन्न (आत्माओं के), गेहे घर में, योगभ्रष्टः-योग से च्युत, अभिजायते-जन्म लेता है।
अनुवाद : पुण्यवान् लोकों को प्राप्त कर के अनेक वर्षों पर्यन्त वहाँ वास कर के योगभ्रष्ट पुरुष पवित्र और ऐश्वर्य-सम्पन्न परिवार में पुनः जन्म लेता है।
व्याख्या : योगभ्रष्ट-योग से पतित । योग में कौशल प्राप्त करने में असफल अथवा वह व्यक्ति जिसने योग के कतिपय सोपानों का आरोहण किया; किन्तु अभ्यास में प्रमाद (शिथिलता) और वैराग्य के अभाव के कारण (माया अथवा इन्द्रियों की दासता का शिकार हो कर) पतित हो गया।
पुण्यकृत् -सत्य-पथ पर अडिग रह कर यज्ञ, दान, अनुष्ठान, देवपूजा और अन्य शास्त्रविहित कर्म करने वाले पुण्यकृत् कहलाते हैं।
शाश्वतीः समाः-शाश्वती का प्रयोग यहाँ नित्य के भाव में नहीं है, प्रत्युत् अपेक्षाकृत दीर्घावधि के लिए प्रयोग हुआ है।
शुचि-पवित्र वे हैं जो शुद्ध, नैतिक जीवन व्यतीत करते हैं। जिनका हृदय परिमार्जित है (ईर्ष्या, घृणा, दम्भ और लोभ से मुक्त है)। (निरूपण- IX.20, 21)
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ।।४२ ।।
शब्दार्थ : अथवा- अथवा, योगिनाम्-योगियों के, एव-ही, कुले कुल में, भवति-जन्म लेता है, धीमताम् - बुद्धिमानों के, एतत् - यह, हि-निश्चित रूप से, दुर्लभतरम् -अत्यन्त दुर्लभ, लोके-लोक में, जन्म-जन्म, यत्-जो, ईदृशम् - इस प्रकार का।
अनुवाद : अथवा वह अत्यन्त बुद्धिमान् योगियों के कुल में जन्म लेता है। निस्सन्देह इस संसार में ऐसा जन्म मिलना अत्यन्त दुर्लभ है।
व्याख्या : पूर्व-श्लोक में वर्णित धार्मिक कुल में जन्म लेने की अपेक्षा बुद्धिमान् योगी के घर जन्म लेना और भी दुर्लभ है।
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।।४३ ।।
शब्दार्थ : तत्र-वहाँ, तम्-उस, बुद्धिसंयोगम् - ज्ञान के संयोग को, लभते-प्राप्त करता है, पौर्वदेहिकम् -पूर्व-जन्म के शरीर में प्राप्त, यतते-यत्न करता है, च-और, ततः उसकी अपेक्षा, भूयः-अधिक, संसिद्धौ-सिद्धि के लिए, कुरुनन्दन-कुरुपुत्र (अर्जुन)।
अनुवाद : हे अर्जुन, वहाँ वह पूर्व-जन्म में संग्रहीत ज्ञान के संयोग में आता है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूर्व की अपेक्षा और अधिक यत्न से साधनारत हो जाता है।
व्याख्या : इस लोक में पुनः जन्म लेने पर योग-मार्ग में पूर्वकृत् अभ्यास और प्रयास विनष्ट नहीं होते। अब वे पूर्ण फल प्रदान करने के लिए उसके भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास में शीघ्रता लाते हैं।
हमारे कर्म और विचार सूक्ष्म संस्कारों के रूप में अवचेतन मन में रहते हैं। संस्कार के रूप में हमारे अनुभव, हमारी प्रकृति और वृत्तियाँ भी अवचेतन मन में संग्रहीत रहती हैं। पूर्व-जन्म के संस्कारों को आगामी जन्म में पुनर्नवा शक्ति और दिव्य चेतना प्राप्त होती है। यौगिक अभ्यास और ध्यान के संस्कार तथा यौगिक वृत्तियाँ साधक को पूर्व-जन्म में किये गये प्रयासों की अपेक्षा और अधिक शक्ति और प्रयास से आगे बढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। अधिकाधिक आध्यात्मिक अनुभव और उच्चतर लोकों के साक्षात्कार के लिए अब वह पूर्व-जन्म में किये गये संघर्ष की अपेक्षा और अधिक संघर्ष और कठोर यत्न करेगा।
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।।४४ ।।
शब्दार्थ : पूर्वाभ्यासेन-पूर्वाभ्यास के द्वारा, तेन-उसके द्वारा, एव-ही, ह्रियते-आकर्षित होता है, हि-निश्चय से, अवशः स्वतः ही, अपि भी, सः- वह, जिज्ञासुः- उत्सुक (योग-विज्ञान का), अपि-भी, योगस्य-योग का, शब्दब्रह्म-शब्दब्रह्म, अतिवर्तते-परे चला जाता है।
अनुवाद : उसी पूर्व के अभ्यास के कारण वह स्वतः ही (विवश-सा हो कर) योग में आकृष्ट किया जाता है। केवल योग का ही जिज्ञासु होने पर भी वह शब्दब्रह्म से अतीत पहुँच जाता है।
व्याख्या : अशुभ कर्मों की प्रबलतावश यौगिक अनुशासन को अपनाने की इच्छा न होते हुए भी पूर्व-जन्म के योगाभ्यास के संस्कारवश, यदि वह साधक उन (संस्कारों) के प्रति सचेत भी न हो, पुनरपि उस योगभ्रष्ट साधक को उस लक्ष्य की ओर प्रेरित किया जाता है, जहाँ वह पहले पहुँचना चाहता था । पूर्व-जन्म में यदि उसने कोई ऐसा बहुत अशुभ कर्म न किया हो जो उसकी यौगिक वृत्तियों को अभिभूत कर ले, तो निश्चित रूप से पूर्व-जन्म में संचित यौगिक संस्कारों वश और अधिक उत्साह से अब योगाभ्यास में उन्नति करेगा। अशुभ कर्म की शक्ति यदि प्रबल है, तो कुछ समय के लिए यौगिक वृत्ति अभिभूत हो जायेगी, दब जायेगी। अशुभ कर्मों के परिणाम क्षीण होते ही यौगिक संस्कारों की अभिव्यक्ति प्रारम्भ हो जायेगी। अब साधक कठोर योगाभ्यास द्वारा अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति करेगा।
एक जिज्ञासु भी, जिसमें योग का ज्ञान प्राप्त करने की आकाङ्क्षा जाग्रत हो गयी हो, शब्दब्रह्म अर्थात् वेदों से भी परे पहुँच जाता है। वह वैदिक प्रक्रियाओं और अनुष्ठानकर्ताओं से भी उत्कृष्टतर हो जाता है। अब वह रूप और विधि-विधानों के जाल से मुक्त हो जाता है। वह मात्र यज्ञादि अनुष्ठानों से सन्तुष्ट नहीं रहता । विषय-वासनाओं से प्राप्त सन्तोष से कहीं उच्चतर तुष्टि की उसे पिपासा रहती है। जो साधक योग के नियमों की प्रकृति मात्र जानने का इच्छुक रहता है, वह स्वयं को शब्दब्रह्म अथवा वैदिक अनुष्ठानों के प्रभाव से मुक्त कर लेता है। एक सामान्य जिज्ञासु की यदि यह दशा हो सकती है, तो सतत योग का अभ्यास करने वाले साधक अथवा निर्विकल्प समाधि में स्थित साधक की प्रोन्नत, उत्कृष्ट दशा तो अनिर्वचनीय ही होगी। वह वैदिक विधि-विधानों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त हो जायेगा। वह शाश्वत आनन्द और शाश्वत शान्ति का सुखास्वाद लेगा जो शाश्वत ब्रह्म से अभेद्य है।
जिस साधक को केवल मोक्ष की आकाङ्क्षा है वह अपरिहार्य, अभीप्सित और नैमित्तिक कर्मों के त्याग अथवा उनके न करने के पाप से प्रभावित नहीं होता। वह शब्दब्रह्म (वेद) से परे पहुँच जाता है।
पूर्व-जन्म के किसी संस्कार के बिना भी यदि यौगिक साधक को यह उच्च अवस्था प्राप्त होती है, तो निस्सन्देह पूर्व-जन्म में संचित योग-संस्कार से युक्त साधक की दशा और भी उन्नत होगी।
पूर्व-जन्म में योगभ्रष्ट और इस जन्म में सभी क्रिया-कलापों को तिलांजलि दे कर योग-मार्ग का अनुसरण करने वाला साधक कितना सौभाग्यशाली होगा ?
मोक्ष की तीव्र इच्छा से प्रेरित हो कर वह इस जन्म में कठोर साधना करता है। पूर्व-जन्म में किये हुए शुभ संस्कारों से मानो विवश (प्रेरित) हो कर वह योगाभ्यास में संलग्न होता है।
इस श्लोक में भगवान् इस सत्य पर बल देते हैं कि योगाभ्यास का कोई भी प्रयास विफल नहीं होता। छोटे-से-छोटा प्रयास भी कभी-न-कभी अपना प्रभाव दिखायेगा, वह चाहे इस जन्म में हो अथवा आगामी जन्म में। अतः मूढ़तम साधक भी इस पथ पर चलने के लिए आशावादी बना रहे, निराश न हो ।
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः ।
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ।।४५ ।।
शब्दार्थ : प्रयत्नात् - कठिन प्रयास से, यतमानः - प्रयास करता हुआ, तु-किन्तु, योगी-योगी, संशुद्धकिल्बिषः- पाप मुक्त हो कर, अनेकजन्मसंसिद्धः - अनेक जन्मों के पश्चात् सिद्धि प्राप्त कर के, ततः- तत्पश्चात्, याति-पहुँचता है, पराम् सर्वोच्च, गतिम् गति को ।
अनुवाद : घोर तपस्या में संलग्न योगी प्रयास करता हुआ, सब पापों से विशुद्ध (मुक्त) हो कर अनेक जन्मों के संस्कारों से क्रमशः सिद्धि प्राप्त कर के परम गति, सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करता है।
व्याख्या : अनेक जन्म में थोड़ा-थोड़ा अनुभव प्राप्त कर के वह अन्ततः सिद्धि को प्राप्त करता है। तत्पश्चात् वह आत्म-ज्ञान प्राप्त कर के जीवन के सर्वोच्च आनन्द में रमण करता है।
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ।।४६ ।।
शब्दार्थ : तपस्विभ्यः- तपस्वियों से, अधिकः-श्रेष्ठ, योगी-योगी, ज्ञानिभ्यः- ज्ञानियों से, अपि-भी, मतः- माना गया है, अधिकः-बढ़ कर, कर्मिभ्यः सकाम कर्म करने वालों से, च-और, अधिकः - श्रेष्ठ, योगी-योगी, तस्मात् - इसलिए, योगी-योगी, भव-बनो, अर्जुन-हे अर्जुन ।
अनुवाद : योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी ही श्रेष्ठ है; अतः हे अर्जुन, योगी बनो।
व्याख्या : तपस्वी-अध्याय XVII. १४, १५ और १६ में उल्लिखित शरीर, मन और वाणी का तप करने वाला तपस्वी है।
ज्ञानी-जिसे शास्त्रों का ज्ञान है अर्थात् परोक्ष ज्ञान अथवा सैद्धान्तिक ज्ञान ।
कर्मि-वैदिक अनुष्ठानों को करने वाला, इन सबसे योगी श्रेष्ठ है; क्योंकि उसे निर्विकल्प समाधि द्वारा अथवा भावातीत ज्ञान द्वारा आत्म-ज्ञान प्राप्त हुआ है। (निरूपण-V.2; XII.12; XIII.24)
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ||४७ ।।
शब्दार्थ : योगिनाम् - योगियों में, अपि-भी, सर्वेषाम् समस्त, मद्गतेन-मेरे परायण, अन्तरात्मना -भीतर से, श्रद्धावान् श्रद्धायुक्त, भजते-भजन करता है, यः जो, माम्-मेरा, सः- वह, मे—मुझे, युक्ततमः- अत्यन्त धर्मशील (पुण्यवान्), मतः माना जाता है।
अनुवाद : समस्त योगियों में भी जो पूर्ण निष्ठावान् हो कर अपनी अन्तरात्मा से मेरी आराधना करता है और मेरे परायण हो गया है, उस योगी को मैं सर्वाधिक युक्त मानता हूँ।
व्याख्या : योगिनामपि सर्वेषाम् - जो मुझ परम पुरुष की पूजा करता है वह वसु, रुद्र, आदित्य आदि देवों की पूजा करने वालों से श्रेष्ठतर है।
मद्गतेनान्तरात्मना मुझमें अपने मन को लीन कर के। (निरूपण-V1.32)
इस अध्याय को आत्मसंयमयोग अथवा अध्यात्मयोग भी कहा जाता है।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ||६ ।।
।। इति ध्यानयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ सप्तमोऽध्यायः
ज्ञानविज्ञानयोगः
श्री भगवानुवाच
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ।।१ ।।
शब्दार्थ : मयि-मुझ में, आसक्तमनाः- आसक्त मन वाला, पार्थ-हे पार्थ, योगम् योग का, युञ्जन् - अभ्यास करते हुए, मदाश्रयः- मेरे आश्रित, असंशयम् निस्सन्देह, समग्रम् - पूर्णतया, माम् -मुझको, यथा-जैसे, ज्ञास्यसि-जानोगे, तत्वह, शृणु सुनो।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : हे अर्जुन, मन को मुझ में एकाग्र कर के, योग का अभ्यास करते हुए और मेरे परायण हो कर निश्चितरूप से तुम मुझे किस प्रकार जानोगे, वह मुझ से सुनो।
व्याख्या: लौकिक वस्तुओं का आकाङ्क्षी पुरुष यज्ञादि अग्निहोत्र करेगा अथवा सकाम भाव से दान दे कर, कुआँ आदि खुदवा कर, अस्पताल बनवा कर, विश्रामगृह आदि बनवा कर यश प्राप्त करेगा। परन्तु योगी इसके विपरीत स्थिरचित्त हो कर योगाभ्यास करेगा और केवल भगवान् की ही शरण में जाएगा। उसका मन सदा भगवान् में स्थिर रहेगा। वह भगवान् के उत्कृष्ट गुणों का चिन्तन करेगा जैसे सर्वशक्तिमानता, सर्वज्ञता, अनन्त प्रेम, सौन्दर्य, कृपा, शक्ति, दया, प्रचुर सम्पत्ति, अक्षय तेज, अनादि महिमा, पवित्रता आदि।
किसी राजा के सेवक का चित्त सतत, राजा की सेवा करते हुए भी उसमें स्थिर नहीं रहता। वह तो अपनी पत्नी और बच्चों का चिन्तन करता रहता है। तुम उस सेवक की भाँति मत बनो। मुझ सर्वव्यापक में अपना मन प्रतिष्ठित करो और केवल मेरी शरण में आओ, अनन्य भाव से । अध्याय VI में दिए गए उपदेशों के अनुरूप मन को नियन्त्रित करने का अभ्यास करो। तब तुम मुझे जान - लोगे और मेरे गुणों का भी ज्ञान तुम्हें पूर्णतया हो जाएगा।
भगवत् गुणगान करने से तुम्हारे भीतर भगवत् प्रेम जागृत और विकसित होगा और तुम्हारा मन मुझ में स्थिर होगा। भगवान् के लिए अनन्य प्रेम ही वास्तविक भक्ति है। निस्सन्देह तुम पूर्ण आत्म-ज्ञान प्राप्त करोगे।
भगवान् का शरणागत और उनमें मन को स्थित रखने वाला अथवा स्थिर करने का अभ्यास करने वाला साधक क्षण भर के लिए भी वियोग सहन नहीं कर सकता।
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ।।२ ।।
शब्दार्थ : ज्ञानम् - शास्त्रों का परोक्ष ज्ञान, ते तुम्हें, अहम् - मैं, सविज्ञानम् -साक्षात्कार सहित अर्थात् आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति सहित, इदम् - यह, वक्ष्यामि बताऊँगा, अशेषतः- पूर्णतया, यत्-जो, ज्ञात्वा-जान कर, न-नहीं, इह-यहाँ, भूयः-पुनः, अन्यत्-और कुछ, ज्ञातव्यम्-जानने योग्य, अवशिष्यते रह जाता है।
अनुवाद : अब मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित (आत्मानुभूति सहित) उस ज्ञान का उपदेश करूँगा जिसे जान कर कुछ और जानने योग्य शेष नहीं रह जाता ।
व्याख्या : उपनिषदों के अध्ययन से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। विज्ञान है विशेष ज्ञान अर्थात् अपरोक्ष ज्ञान अथवा आत्म ज्योतित ज्ञान (सहजावबोध) ।
इस श्लोक में भगवान् ज्ञान की प्रशंसा करते हैं ताकि अर्जुन उनके उपदेश को हर्षोन्मत्त हो कर विश्वास (निष्ठा) और रुचि के साथ श्रवण करे। भगवान् कहते हैं- "मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूँगा। तुम आत्मा का पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञता को प्राप्त करोगे जिसे जान कर इस लोक में और कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता ।" आत्म-ज्ञान प्राप्त कर के सर्वस्व ज्ञान हो जाता है। इसीलिए तो शौनक, एक महान गृहस्थी होते हुए भी अङ्गिरस के पास आदर सहित जा कर बोले-"भगवन्, वह कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान हो जाने पर सब कुछ जानने में आ जाता है?" (निरूपण –XIII. 11)
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।।३ ।।
शब्दार्थ : मनुष्याणाम् - मनुष्यों में, सहस्रेषु सहस्रों में, कश्चित् -कोई, यतति-यत्न करता है, सिद्धये-सिद्धि के लिए, यतताम्-यत्न करने वालों में, अपि-भी, सिद्धानाम् - सिद्धि प्राप्त पुरुषों में, कश्चित्-कोई, माम्-मुझे, वेत्ति-जानता है, तत्त्वतः तत्त्व (सार) रूप से।
अनुवाद : सहस्रों मनुष्यों में कोई विरल ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है और उन सिद्धि प्राप्त सफल पुरुषों में भी कोई विरला ही मुझे तत्त्व रूप से जान पाता है।
व्याख्या : तत्त्व रूप से आत्म-ज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नितान्त दुर्लभ है।
सिद्धानाम् - पूर्णता प्राप्त सिद्ध पुरुष । किन्तु यहाँ इसका अभिप्राय है पूर्णता प्राप्ति का यत्न करने वाले ।
हीरे, माणिक, मोती के क्रेता कम हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले कम हैं, इसी प्रकार आत्म-साक्षात्कार के लिए प्रयासरत और उनमें भी सत्य के तत्त्ववेत्ता बहुत कम हैं। जीवन्मुक्त विरल हैं।
शाश्वत शान्ति, अक्षय सुख, शाश्वत आनन्द और अमरत्व के असंख्य फलों की वृष्टि आत्म-ज्ञानी पर होती है। किन्तु एक योग्य और सच्चा आध्यात्मिक साधक जो दृढ़ संकल्प और लौह निश्चय वाला है, मोक्ष के साधन चतुष्टय (अध्याय ३, श्लोक ३) से युक्त है वह आत्म-ज्ञान सहज ही प्राप्त कर सकता है।
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।।४ ।।
शब्दार्थ : भूमिः पृथ्वी, आपः-जल, अनल:-अग्नि, वायुः- वायु, खम् - आकाश, मनः मन, बुद्धिः बुद्धि, एव-ही, च-और, अहंकार: अहंकार, इति-इस प्रकार, इयम्-यह, मे-मेरी, भिन्ना-विभक्त, प्रकृतिः- प्रकृति, अष्टधा-आठ प्रकार की।
अनुवाद : पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार-यह मेरी आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है।
व्याख्या : यह अष्टधा प्रकृति निम्न अथवा अपरा प्रकृति है। पाँच स्थूल तत्त्वों का विकास पञ्चीकरण की प्रक्रिया से तन्मात्राओं (मूल तत्त्वों) से होता है। तन्मात्रायें सूक्ष्म मूल तत्त्व हैं। इस श्लोक में पृथ्वी, जल आदि सूक्ष्म मूल तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे पाँच स्थूल तत्त्वों का उद्भव हुआ है।
मन अपने मूल कारण अहंकार का द्योतक है, बुद्धि अपने कारण महत् की द्योतक है। अहंकार अव्यक्त मूल प्रकृति का द्योतक है जो अविद्या एवं सब प्रकार की वासनाओं व सुप्त वृत्तियों से संयुक्त है। प्रत्येक मनुष्य के समस्त कर्मों का कारण अहंकार (अहं भाव) है और क्योंकि मनुष्य में अहंकार ही वह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जिस पर अन्य सभी तत्त्व निर्भर हैं, अतः अहंकारयुक्त 'अव्यक्तम्' ही यहाँ पर 'अहंकार' संज्ञा से अभिहित है क्योंकि विषयुक्त भोजन विष ही कहलाता है।
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ।।५ ।।
शब्दार्थ : अपरा-निम्न, इयम्-यह, इतः- यहाँ से, तु-लेकिन, अन्याम् -पृथक्, प्रकृतिम् -प्रकृति को, विद्धि-जानो, मे—मेरी, पराम् उच्च, जीवभूताम् - जीव-रूपा, महाबाहो - हे महाबाहो, यया-जिसके द्वारा, इदम् यह, धार्यते-धारण किया जाता है, जगत् संसार ।
अनुवाद : हे अर्जुन, यह अपरा (निम्न) प्रकृति है। मेरी उच्चतर परा प्रकृति को पृथक् जानो जो जीवभूता है अर्थात् चेतन है और जिसके द्वारा यह जगत् धारण किया जाता है।
व्याख्या : पूर्व श्लोक में विवेचित अष्टधा प्रकृति निम्नतर प्रकृति कही गई है। यह क्षेत्र है, जड़ पदार्थ है, अशुद्ध है। बुराई को जन्म दे कर यह बन्धन का कारण बनती है। किन्तु उच्चतर प्रकृति पवित्र है। यह मेरी ही आत्मा है, क्षेत्रज्ञ (क्षेत्र को जानने वाला आत्म-तत्त्व) है जिसके द्वारा जीवन को पोषण मिलता है और जो समस्त जगत् में व्याप्त हो कर इसे धारण किए रहता है। यह जीवन-तत्त्व है, आत्म-चेतना है जो ब्रह्माण्ड को धारण करती है।
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।।६ ।।
शब्दार्थ : एतत् -यह, योनीनि-योनियाँ, भूतानि-प्राणी, सर्वाणि- समस्त, इति-इस प्रकार, उपधारय-जानो, अहम् -मैं, कृत्स्नस्य-सारे, जगतः - जगत् का, प्रभवः -मूल स्रोत, प्रलयः -प्रलय, तथा-भी।
अनुवाद : इन दोनों प्रकृतियों को समस्त प्राणियों की योनियाँ ही समझो। अतः मैं ही इस जगत् का उद्भव और प्रलय हूँ।
व्याख्या : निम्नतर और उच्चतर प्रकृतियाँ समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाली हैं। इन प्रकृतियों का मूल स्रोत होने के कारण मैं इस ब्रह्माण्ड का कारण हूँ। मुझसे ही यह जगत् अस्तित्वमान हो कर मुझ में ही लीन हो जाता है।
ब्रह्मसूत्र (अध्याय १, खखण्ड १, सूत्र २) में कहा है- "जन्माद्यस्य यतः" अर्थात् ब्रह्म ही वह सर्वज्ञ सर्वव्यापक सत्ता है जिससे विश्व का उद्भव, विकास और विलयन होता है।
जिस प्रकार मन स्वप्न जगत् का द्रष्टा भी है और उपादान कारण भी है उसी प्रकार से ईश्वर इस जगत् का द्रष्टा और उपादान कारण दोनों ही है। वह निमित्त कारण भी है। निरूपण -XIV.3.
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।।७ ।।
शब्दार्थ : मत्तः मुझ से, परतरम् - उच्चतर, न-नहीं, अन्यत् अन्य, किश्चित् -कुछ, अस्ति-है, धनञ्जय- हे धनञ्जय, मयि-मुझमें, सर्वम् -सब, इदम् -यह, प्रोतम् -पिरोया हुआ, सूत्रे -धागे में, मणिगणाः मणियाँ, इव-समान ।
अनुवाद : हे धनञ्जय, संसार में मुझ से उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है। सूत्र में मणियों के सदृश ये सब मुझ में पिरोया हुआ है।
व्याख्या : विश्व का मूल कारण मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। केवल मैं ही संसार का उत्पादक हूँ। सूत्र और मणियों की उपमा इस सत्य को प्रकाशित करती है कि सब प्राणी और समस्त संसार भगवान् रूपी सूत्र में गुंथा हुआ है। (सूत्र ने मणियों को मिला कर रखा है)। यहाँ सूत्र मणियों का कारण नहीं है। ब्रह्म ही सर्वस्व है, उससे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं।
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ।।८ ।।
शब्दार्थ : रसः- रस, अहम् -मैं, अप्सु-जल में, कौन्तेय-हे कुन्ती पुत्र, प्रभा-प्रकाश, अस्मि (मैं) हूँ, शशिसूर्ययोः सूर्य और चन्द्रमा में, प्रणव -ओ३म्, शब्द, सर्ववेदेषु सब वेदों में, शब्दः- ध्वनि, खे-आकाश में, पौरुषम् -पुरुषत्व, नृषुनरों में।
अनुवाद : हे अर्जुन, जलों में रस (स्वाद) मैं हूँ, सूर्य और चन्द्र में प्रकाश मैं हूँ, “” शब्द मैं हूँ, आकाश में ध्वनि मैं हूँ और पुरुषों में पौरुष मैं हूँ।
व्याख्या : मुझ में समस्त प्राणी और पूर्ण विश्व इसी प्रकार गुम्फित है जैसे वस्त्र में बुनाई का ताना। स्वाद के रूप में मुझ में जल गुम्फित है, प्रकाश के रूप में सूर्य और चन्द्र, ओंकार के रूप में समस्त वेद और पुरुषत्व के रूप में सब पुरुष मुझ में गुम्फित हैं।
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।।९ ।।
शब्दार्थ : पुण्यः मधुर, गन्धः गन्ध, पृथिव्याम् -पृथ्वी में, च-और, तेजः-तेज, च-और, अस्मिㅡ (मैं) हूँ, विभावसौ-अग्नि में, जीवनम् - जीवन, सर्वभूतेषु सब प्राणियों में, तपः-तप, च-और, अस्मि-हूँ, तपस्विषु- तपस्वियों में।
अनुवाद : पृथ्वी में मधुर गन्ध मैं हूँ, अग्नि में तेज (उष्मा) मैं हूँ, प्राणियों का जीवन मैं हूँ और तपस्वियों का तप मैं हूँ।
व्याख्या : सुगन्ध रूप में पृथ्वी मुझ में ग्रथित है, तेज रूप में अग्नि गुम्फित है, जीवन रूप में सब प्राणी मुझ में गुम्फित हैं और तप रूप में सब तपस्वी मुझ में गुम्फित हैं। मैं प्रत्येक वस्तु का अधिष्ठान हूँ, आश्रय हूँ।
मैं वह शक्ति हूँ जो तपस्वियों को मन तथा इन्द्रियों के नियन्त्रण में सहायता करती है।
कृष्ण कहते हैं-"मैं रुचिकर सुगन्ध हूँ।" यदि अर्जुन प्रश्न करते -"तो अरुचिकर सुगन्ध कौन है?" तो कृष्ण का उत्तर होता- "वह भी मैं ही हूँ।"
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।।१० ।।
शब्दार्थ : बीजम् बीज, माम्-मुझे, सर्वभूतानाम् -सब प्राणियों का, विद्धि-जानो, पार्थ-हे पार्थ, सनातनम् -सनातन, बुद्धिः बुद्धि, बुद्धिमताम् – बुद्धिमानों में, अस्मि-हूँ, तेजः-तेज, तेजस्विनाम् - तेजस्वियों का, अहम् -मैं।
अनुवाद : हे अर्जुन, सब प्राणियों का शाश्वत बीज मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ।
व्याख्या : बीज का अभिप्राय "कारण" से है।
तेजस्, विक्रान्त पुरुष अथवा शूरवीरता (पराक्रम) के भाव में भी प्रयोग होता है।
अर्जुन यदि पूछते-"आपका बीज कौन है?" तो भगवान् कहते-"मेरा कोई बीज नहीं। मैं सब का स्रोत हूँ। मैं कारणरहित कारण हूँ। मैं आदि पुरुष हूँ।"
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् ।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।।११ ।।
शब्दार्थ : बलम् बल, बलवताम्-बलवानों का, च-और, अहम् - मैं, कामरागविवर्जितम् - इच्छा और आसक्ति से रहित, धर्माविरुद्धः -धर्म के अनुकूल, भूतेषु प्राणियों में, कामः-कामना, अस्मिㅡ(मैं) हूँ, भरतर्षभ हे भरतश्रेष्ठ ।
अनुवाद : बलवानों में मैं आसक्ति और कामरहित बल हूँ और हे अर्जुन, सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ।
व्याख्या : कामः - इन्द्रियों के सम्पर्क में आने वाले विषयों की इच्छा।
रागः - इन्द्रियों के सम्पर्क में आने वाले विषयों में आसक्ति ।
शरीर के पोषण के लिए अनिवार्य बल मैं हूँ। मैं वह शक्ति या बल नहीं . जो ऐन्द्रिक विषयों के प्रति काम-वासना और आसक्ति उत्पन्न करे जैसा कि सांसारिक व्यक्तियों के साथ है। मैं शास्त्रों की आज्ञा के अनुरूप अथवा जीवन के कर्तव्यों के नियमों के अनुरूप उपदिष्ट काम हूँ। सन्तुलित खान-पान की कामना मैं हूँ जो शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है और योगाभ्यास में सहायक है।
ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।। १२ ।।
शब्दार्थ : ये जो भी, चऔर, एव-ही, सात्त्विकाः-शुद्ध, भावाः- भाव, राजसाः-क्रियाशील, तामसाः- जड़, च-और, ये-जो भी, मत्तः- मुझ से, एव-ही, इति-इस प्रकार, तान् - उन्हें, विद्धि-जानो, न-नहीं, तु-निश्चय से, अहम् -मैं, तेषु उनमें, ते-वे, मयि मुझमें।
अनुवाद : संसार में जो भी प्राणी (अथवा पदार्थ) सात्त्विक (शुद्ध) भाव वाले हैं अथवा राजसिक (क्रियाशील) भाव वाले हैं अथवा तामसिक (जड़) भाव में हैं उन सब को तुम मुझ से उत्पन्न हुआ जानो। वे मुझ में हैं किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ।
व्याख्या : यह सृष्टि त्रिगुणमयी है-सत्त्व, रजस् और तमस्। सभी जड़-चेतन पदार्थ प्रकृति के इन तीन गुणों का समाहार (समुदाय) हैं। उनमें एक गुण प्रधान होता है और वह प्रधान गुण वस्तु विशेष अथवा व्यक्ति को स्वभाव अथवा सहज गुण प्रदान करता है।
देवों में, तपस्वियों में, दुग्ध और हरे अनाज में सत्त्व गुण प्रधान होता है। गन्धर्व, राजा, योद्धा और मिर्च रजस् गुण प्रधान है। राक्षस, शूद्र, लहसुन, प्याज और मांस तमस् प्रधान हैं।
यद्यपि ये जीव और पदार्थ मुझसे ही उत्पन्न हैं तथापि मैं उनमें नहीं हूँ। मैं स्वतन्त्र हूँ। मैं उनका आधार हूँ, वे मुझमें हैं अतः मुझ पर वैसे ही निर्भर हैं जैसे रस्सी में आरोपित सर्प। सर्प तो रज्जु में है किन्तु रज्जु कभी सर्प में नहीं है। सिन्धु में लहरें हैं किन्तु लहरों में सिन्धु तो नहीं हो सकता। (निरूपण-IX.4,6)
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ।।१३ ।।
शब्दार्थ : त्रिभिः - तीनों के द्वारा, गुणमयैः- गुणों से युक्त, भावैः- भावों के द्वारा, एभिः- इन के द्वारा, सर्वम् -समस्त, इदम् - यह, जगत् संसार, मोहितम् -मोहग्रस्त, न-नहीं, अभिजानाति-जानता, माम् -मुझे, एभ्यः- इन से, परम् - उच्चतर, अव्ययम् सनातन ।
अनुवाद : प्रकृति के इन गुणों से मोहित संसार उनसे पृथक् मुझ परम अविनाशी को नहीं जानता।
व्याख्या : इस जगत् के लोग माया (प्रकृति) के तीन गुणों से मोहित हैं। स्नेह, आसक्ति और मोहग्रस्त प्रेम इन तीन गुणों के परिवर्तित रूप हैं। इन तीनों गुणों द्वारा सृजित मोह के कारण मनुष्य लौकिक बन्धन तोड़ने में असमर्थ है और अपने मन को इन तीन गुणों के स्वामी भगवान् की ओर उन्मुख करने में भी असमर्थ है।
अव्यय-अक्षय, अविनाशी, अपरिवर्तनशील । आत्म-तत्त्व एक समन्वित सार-तत्त्व है। शरीर में आने वाले षड् भाव विकार इसमें नहीं आते जैसे-अस्तित्व, जन्म, विकास, परिवर्तन, क्षय और मृत्यु । (निरूपण-VII. 25)
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।।१४ ।।
शब्दार्थ : दैवी-दिव्य, हि-निश्चयेन, एषा-यह, गुणमयी-गुणयुक्त, मम मेरी, माया-माया (भ्रम), दुरत्यया-पार करने में कठिन, माम् मुझको, एव-ही, ये-जो, प्रपद्यन्ते-शरण में आते हैं, मायाम् -माया को, एताम् -इस, तरन्ति-तर जाते हैं, ते वे।
अनुवाद : निश्चित रूप से प्रकृति के तीन गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य माया को जीतना कठिन है। वे लोग माया को पार कर जाते हैं जो मेरी शरण में आते हैं।
व्याख्या : माया भगवान् का कारण शरीर है और विश्व का स्थूल कारण है। यह ईश्वर में प्रतिष्ठित है अर्थात् ईश्वर का नैसर्गिक भाव है। यह सत्त्व, रजस् और तमस् तीन गुणों से युक्त है। सब धर्मों (कर्मों) का त्याग कर जो पूर्णतया ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं वे सब को भ्रमित करने वाली इस माया को पार कर जाते हैं। वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।
ईश्वर मायापति हैं। उनका इस पर पूर्ण नियन्त्रण है। अविद्या जीवात्मा की उपाधि है। जीव इस अज्ञान का दास है। सच्चिदानन्द ब्रह्म से जीव को पृथक् करने वाला आवरण अज्ञान ही है। ज्ञानोदय होने पर जीव अपने जीवत्व का त्याग कर के ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है। (निरूपण-XV. 3, 4.)
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ।।१५ ।।
शब्दार्थ : न -नहीं, माम् -मुझे, मेरी, दुष्कृतिनः - पापकर्मी, मूढाः - मूर्ख, भ्रमित, प्रपद्यन्ते-शरण ग्रहण करते हैं, नराधमाः- अधम व्यक्ति, मायया-माया से, अपहृतज्ञाना:-जिनका ज्ञान हरा गया है, आसुरम्-आसुरी (राक्षसी), भावम् - भाव को, आश्रिताः आश्रित ।
अनुवाद : अशुभ कर्म करने वाले और मूढ़ लोग जो नरों में अधम हैं, मेरी शरण में नहीं आते। मायावश जिनके ज्ञान का हरण हो चुका है वे आसुरी मार्ग का अनुसरण करते हैं।
व्याख्या : इन तीन प्रकार के लोगों में उचित-अनुचित, सत्य-असत्य का विवेक नहीं होता। वे हिंसा, चोरी, डकैती तथा अन्य क्रूर कृत्य करते हैं। वे दूसरों को अनेक प्रकार से हानि पहुँचाते हैं और असत्य भाषण करते हैं।
आसुरी वृत्ति को अपनाने वाले विरोचन की भाँति शरीर को ही आत्मा मान कर पुष्प, सुगन्धि, लेप, सुन्दर वस्त्र और रुचिकर (स्वाद) व्यञ्जनों से इसकी पूजा करते हैं। वे भ्रमित आत्माएँ हैं। वे शरीर के पोषण हेतु अनेक प्रकार के बुरे कर्म करते हैं। अतः वे मेरी आराधना नहीं करते। अविद्या ही इन सभी बुराइयों का मूल है। (निरूपण –XVI. 16, 20)
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।।१६ ।।
शब्दार्थ : चतुर्विधाः- चार प्रकार के, भजन्ते-पूजा करते हैं, माम् -मेरी, जनाः- लोग, सुकृतिनः पुण्यात्मा, अर्जुन-हे अर्जुन, आर्तः-दुःखी, जिज्ञासुः- जिज्ञासु, अर्थार्थी-सम्पत्ति की कामना वाले, ज्ञानी-ज्ञानी, च-और, भरतर्षभ-हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ ।
अनुवाद : हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यकर्मी मेरी आराधना करते हैं। वे हैं-आर्त (दुःखी), जिज्ञासु (ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक), अर्थार्थी (धन का इच्छुक) और ज्ञानी ।
व्याख्या : आर्त वह है जो किसी पुराने असाध्य रोग से पीड़ित है, भूकम्प से, ज्वालामुखी फूटने से, मेघगर्जना से, डकैती अथवा शत्रु के आक्रमण से अथवा वन्य पशु के आक्रमण आदि से जिसके प्राण संदिग्ध हैं (जीवन संशय में है)। आर्तावस्था में द्रौपदी और गजेन्द्र ने भगवान् को पुकारा। यह आर्त भक्ति के दृष्टान्त हैं।
जिज्ञासु अन्वेषक है। वह इस संसार से असन्तुष्ट है। उसके जीवन में शून्यता है। वह सदा यही सोचता है कि भौतिक सुखों में वास्तविक आनन्द का अभाव है। पवित्र शाश्वत आनन्द की खोज तो आभ्यंतर में करनी है जो दुःख और शोक से मुक्त करने वाली है। जनक और उद्धव ऐसे ही भक्त थे।
अर्थार्थी वह है जिसे धन-वैभव, स्त्री, बच्चे, पद, नाम और यश की तृष्णा है। सुग्रीव, विभीषण, उपमन्यु और ध्रुव इसी प्रकार के भक्त थे।
ज्ञानी ज्ञान की इच्छा रखने वाले होते हैं जिन्होंने आत्म-ज्ञान प्राप्त किया। शुकदेव जी का नाम इस श्रेणी में लिया जाता है, वे ज्ञानी भक्त थे।
कंस, शिशुपाल और रावण सतत भय और घृणाभाव से भगवत् चिन्तन करते थे। वे वैर भक्तियुक्त भक्त थे।
तुम्हारा उद्देश्य कुछ भी हो, भगवान् के प्रति निष्ठावान् बनो । समय के साथ तुम्हारी निष्ठा, भक्ति तुम्हारे उद्देश्य को भी परिष्कृत कर देगी।
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ।।१७ ।।
शब्दार्थ : तेषाम् उनमें से, ज्ञानी-ज्ञानी, नित्ययुक्तः - नित्यस्थित, एकभक्तिः- एक में भक्तिभाव वाला, विशिष्यते-विशिष्ट है, प्रियः - प्रिय, हि-निश्चय से, ज्ञानिनः- ज्ञानी का, अत्यर्थम् अत्यधिक, अहम् -मैं, सः- वह, च-और, मम-मेरा, प्रियः - प्रिय ।
अनुवाद : उनमें से नित्ययुक्त और एक परमात्मा में भक्तिभाव वाला ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यधिक प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय है।
व्याख्या : 'एकभक्तिः' का अभिप्राय है अविचल अनन्यमनस्क भक्ति-परमात्मा के लिए।
ज्ञानी भक्त सब मत-मतान्तरों, धर्म और समाज के नियमों से परे होता है। ज्ञानी अन्य भक्तों की अपेक्षा श्रेष्ठतर है क्योंकि वह केवल एक परमात्मा में निष्ठा वाला और सतत समन्वित होता है। क्योंकि मैं ही उसका अन्तरात्मा हूँ इसलिए उसको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ। प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मा को सर्वाधिक प्रेम करता है। सबको आत्मा प्रिय है। ज्ञानी मनुष्य मेरी आत्मा है और वह मुझे प्रिय भी है। (निरूपण - II.49; IX.29; XII.14,17,19)
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ।।१८।।
शब्दार्थ : उदाराः-उदार, सर्वे-सब, एव-ही, एते-ये, ज्ञानी-ज्ञानी, तु-किन्तु, आत्मा-आत्मा, एव-ही, मे—मेरा, मतम् -मत, आस्थितः - स्थित, सः- वह, हि-निश्चय से, युक्तात्मा-योग में स्थित पुरुष, माम् -मुझे, एव-ही, अनुत्तमाम् -सर्वोच्च, गतिम् लक्ष्य ।
अनुवाद : ये सभी निश्चित रूप से अच्छे हैं किन्तु मैं ज्ञानी को अपना ही आत्मा मानता हूँ क्योंकि ज्ञानी संयत मन से परम लक्ष्य स्वरूप मुझ में ही प्रतिष्ठित है।
व्याख्या : क्या अन्य तीन प्रकार के भक्त भगवान् को प्रिय नहीं हैं? वे प्रिय हैं। वे सभी उदार हैं। परन्तु, क्योंकि ज्ञानी का मन स्थिर होता है, वह भगवान् में स्थित रहता है इसलिए वह अधिक प्रिय है। परमात्मा के अतिरिक्त उसे अन्य किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं होती। उसका परम लक्ष्य परब्रह्म है। वह अहंग्रह उपासना (सब को अपनी आत्मा के रूप में देखना) करता है। वह यह समझने का प्रयास करता है कि वह ब्रह्म से अभिन्न है इसीलिए ज्ञानी को मैं अपना ही आत्मा मानता हूँ। (निरूपण - II.49)
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।।१९ ।।
शब्दार्थ : बहूनाम् - अनेक, जन्मनाम्-जन्मों के, अन्ते-अन्त में, ज्ञानवान् ज्ञानी, माम् -मेरी, प्रपद्यते - शरण लेता है, वासुदेवः वासुदेव, सर्वम् सर्वस्व, इति-इस प्रकार, सः- वह, सुदुर्लभः -पाना कठिन । महात्मा-महान् आत्मा,
अनुवाद : अनेक जन्मों के उपरान्त ज्ञानी मेरी शरण में आता है किन्तु "वासुदेव ही सर्वस्व है" ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाला महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।
व्याख्या : वसुदेव का पुत्र होने के कारण भगवान् कृष्ण को वासुदेव भी कहा जाता है। वह सर्वव्यापक ब्रह्म हैं।
साधक योगाभ्यास, निःस्वार्थ सेवा, भक्ति और अविराम ध्यान के द्वारा क्रमशः विकास करता है और अनेक जन्म पर्यन्त यह साधना करने के उपरान्त अन्तरात्मा का साक्षात्कार करता है। वह जान लेता है कि वासुदेव ही सर्वस्व है। ऐसी महान् आत्मा का पाना अत्यन्त कठिन है जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो । उसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। यही कारण है कि भगवान् ने कहा है- “सहस्रों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन सफल साधकों में भी कोई विरला ही मुझे तत्त्व रूप से जान पाता है।" (निरूपण-VII.3)
कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।।२० ।।
शब्दार्थ : कामैः-कामनाओं के द्वारा, तैः तैः-उन-उन, हृतज्ञाना:-जिनका ज्ञानहरण हो गया है, प्रपद्यन्ते-शरण में आते हैं, अन्यदेवताः- अन्यदेवता, तम् तम् उस उस, नियमम् -नियम को, आस्थाय अनुसरण कर के, प्रकृत्या-स्वभाव से, नियताः-नियत, स्वया-अपने ही।
अनुवाद : इधर-उधर की इच्छाओं के द्वारा जिनके ज्ञान का हरण हो चुका है वे अपने-अपने स्वभाव के कारण अन्य विधि-विधान करते हुए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं।
व्याख्या : तुच्छ सिद्धियों की प्राप्ति के इच्छुक, धन-वैभव, सन्तान की इच्छा वाले, विवेक शून्य होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित हो कर अपने स्वभाव के अनुरूप वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि अन्य देवों की शरण में जाते हैं। वे इन निम्न देवों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। (निरूपण -IX.23)
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ।।२१ ।।
शब्दार्थ : यः यः जो-जो, याम् याम् -जिस-जिस, तनुम् स्वरूप को, भक्तः - भक्त, श्रद्धया श्रद्धा से, अर्चितुम् -पूजा के लिए, इच्छति-इच्छा करता है, तस्य तस्य-उस-उस की, अचलाम्-अचल, श्रद्धाम्-श्रद्धा को, ताम् उसमें, एव-ही, विदधामि-स्थिर करता हूँ, अहम् - मैं।
अनुवाद : भक्त जिस किसी स्वरूप की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है उसी स्वरूप में उसकी निष्ठा को मैं स्थिर और अचल करता हूँ।
व्याख्या : तनु अर्थात् शरीर शब्द देवता के भाव में प्रयुक्त हुआ है। अन्तर्यामी भगवान्, भक्त के पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसकी निम्न कोटि के देवों के प्रति निष्ठा को स्थिर और अचल करते हैं। (निरूपण - IV.11; IX.22,23)
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ।।२२ ।।
शब्दार्थ : सः वह, तया-उसके, श्रद्धया-विश्वास से, युक्तः युक्त, तस्य-उसकी, आराधनम् -पूजा, ईहते-आकाङ्क्षा करता है, लभते - प्राप्त करता है, च-और, ततः-उससे, कामान्-इच्छाओं को, मया-मेरे द्वारा, एव-निश्चित रूप से, विहितान् - आदिष्ट, हि-निश्चय से, तान्—उन ।
अनुवाद : उस श्रद्धा से युक्त हो कर वह उस देवता के स्वरूप की आराधना में लगता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किये गये उन इच्छित भोगों को निःसन्देह प्राप्त करता है।
व्याख्या : अन्तिम दो शब्द 'हि' और 'तान्' एक शब्द माना जाता है अर्थात् 'हितान्' जिसका अभिप्राय है लाभ । यह अन्य व्याख्या है। निम्न देवताओं की पूजा करने वाला भक्त आकांक्षित फलों की प्राप्ति करता है जिनमें छोटी-मोटी आध्यात्मिक शक्तियाँ निहित हैं। वे पदार्थ भगवान् के आदेश से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि केवल वे ही कर्म और उसके फल के सम्बन्ध को जानते हैं और क्योंकि वे ही सभी प्राणियों की अन्तरात्मा के स्वामी हैं। मूढ़ अथवा अविवेकी पुरुष ही इन अन्य पदार्थों को प्राप्त करने की कामना करते हैं जो कि पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। दयनीय है उनका भाग्य। उनमें विचार-शक्ति नहीं है, समुचित ज्ञान नहीं है। आत्मा रूपी अमोघ हीरा प्राप्त करने की अपेक्षा वे काँच के टुकड़े एकत्र करने में लगे रहते हैं।
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।। २३ ।।
शब्दार्थ : अन्तवत् - अनित्य, तु-निश्चित रूप से, फलम् -फल, तेषाम् उनका, तत् वह, भवति-होता है, अल्पमेधसाम् - अल्प बुद्धि वालों का, देवान् -देवताओं को, देवयज:-देवताओं को पूजने वाले, यान्ति-जाते हैं, मद्भक्ताः - मेरे भक्त, यान्ति-जाते हैं, माम् -मुझको, अपि-भी।
अनुवाद : निस्सन्देह अल्प बुद्धि वालों का प्राप्त फल भी क्षणभङ्गुर होता है। देवताओं को पूजने वाले उन्हें ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं।
व्याख्या : दोनों प्रकार की साधना भक्ति में प्रयास तो वही एक ही है पुनरपि परम पुरुष को पूजने का प्रयास नहीं करते जिससे वे मोक्ष रूप अनन्त फल की प्राप्ति कर सकें। निम्न देवताओं की पूजा का फल भी जो अल्पज्ञों को प्राप्त होता है, वह अल्प, नाशवान् और अनित्य है।
यज्ञ (वैदिक अनुष्ठान), होम (अग्निहोत्र, जिसमें अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं) और विभिन्न प्रकार की तपस्या साधक पर क्षणिक फल की वृष्टि कर सकती हैं, नित्य नहीं। आवागमन के चक्र से मुक्ति ही नित्य आनन्द और शाश्वत शान्ति देने में सक्षम है।
इन्द्रादि देवताओं की पूजा करने वाले साधक सात्त्विक हैं। यक्ष और राक्षसगणों की पूजा करने वाले राजसिक हैं और भूत-प्रेत आदि अशरीरी आत्माओं को पूजने वाले तामसिक होते हैं।
निम्न देवों को पूजने वालों का ज्ञान आंशिक और अपूर्ण होता है। यह मोक्ष प्रदायक नहीं है। (निरूपण-IX.25)
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ।।२४ ।।
शब्दार्थ : अव्यक्तम् अव्यक्त, अप्रकट, व्यक्तिम् - प्रकट स्वरूप को, आपन्नम् - प्राप्त हुए, मन्यन्ते-मानते हैं, माम् -मुझे, अबुद्धयः - बुद्धिहीन, परम् -सर्वोच्च, भावम् सत्ता, अजानन्तः- न जानते हुए, मम-मेरी, अव्ययम् - अनश्वर, अनुत्तमम् - उत्कृष्ट ।
अनुवाद : मेरी उच्चतर, निर्विकार और उत्कृष्ट प्रकृति को न जानते हुए अल्पज्ञ मुझ अव्यक्त को, व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ समझते हैं।
व्याख्या : अज्ञानी मनुष्य भगवान् कृष्ण को एक सामान्य पुरुष मानते हैं। वे सोचते हैं कि पूर्व जन्म की कर्म की शक्ति से भगवान् ने अव्यक्त अवस्था से प्रकट हो कर सामान्य मनुष्यों की भाँति शरीर धारण किया है। उन लोगों को भगवान् की उच्चतर, अनश्वर, स्वयं प्रकाशित प्रकृति का सर्वोच्च सत्ता के रूप में होने का ज्ञान नहीं है। वे मानते हैं कि वे अभी सत्ता में आये हैं जब कि वे सत् स्वरूप हैं, शाश्वत, अनादि, अनन्त, जन्म से परे, मृत्यु से परे, अपरिवर्तनशील, पञ्चातीत, असीमित और अव्यक्त हैं।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।।२५ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, अहम् - मैं, प्रकाशः व्यक्त, सर्वस्य सब का, योगमायासमावृतः योगमाया से आवृत, मूढः- मूर्ख, अयम्-यह, न नहीं, अभिजानाति -जानता है, लोकः संसार, माम् -मुझे, अजम् - जन्मरहित, अव्ययम् - अनश्वर ।
अनुवाद : अपनी योगमाया से आवृत होने के कारण मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता अर्थात् सब के समक्ष प्रकट नहीं होता। ये भ्रमित लोग मुझ जन्मरहित अविनाशी को नहीं जानते ।
व्याख्या : मैं सब मनुष्यों के समक्ष प्रत्यक्ष नहीं हूँ किन्तु जो भक्त केवल मेरी शरण में आते हैं उन विशेष भक्तों के समक्ष मैं प्रकट होता हूँ। मैं उन लोगों को दर्शन नहीं देता जो प्रकृति के तीन गुणों और विरोधी द्वन्द्वों से भ्रमित हैं तथा इस संसार में लिप्त हैं, जो मात्र प्रकृति के गुणों की अभिव्यक्ति, मेरी योगमाया अथवा मेरी सृजनात्मक शक्ति का भ्रम है। यह सांसारिक मनुष्यों की बुद्धि को आवृत कर देती है, अतएव वे भगवान् को नहीं देख सकते जिनके पूर्ण नियन्त्रण में यह माया की शक्ति है।
प्रकृति के तीन गुणों का समाहार योगमाया है। उसके द्वारा प्रसारित भ्रम अथवा आवरण, योगमाया है। सांसारिक व्यक्ति इन तीनों गुणों से उत्पन्न भ्रम से मोहित हैं। इसीलिए वे भगवान् को जानने में सक्षम नहीं हैं जो अजन्मा और निर्विकार हैं।
योगमाया भगवान् के पूर्ण वश में है। ईश्वर इस माया को धारण करता है इसलिए यह अपने ही ज्ञान को तमोवृत नहीं कर सकता। एक जादूगर का सृजित भ्रम जैसे उसे ही धोखा नहीं दे सकता अथवा उसकी अपनी ज्ञान शक्ति को दुर्बाध नहीं कर सकता वैसे ही जो भ्रम भौतिक प्राणियों को बन्धन में डालता है वह भगवान् को किंचित् मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि माया तो पूर्ण रूप से भगवान् के वश में है। (निरूपण - VII. 13; IX.5; X.7; ΧΙ.8)
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।।२६ ।।
शब्दार्थ : वेद जानता हूँ, अहम् -मैं, समतीतानि व्यतीत हुए, वर्तमानानिवर्तमान को, च-और, अर्जुन-हे अर्जुन, भविष्याणि-भविष्य के, च-और, भूतानि प्राणी, माम् -मुझे, तु-लेकिन, वेद-जानता है, न नहीं, कश्चन-कोई भी।
अनुवाद : हे अर्जुन, मैं अतीत में हो चुके, वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ किन्तु मुझे कोई नहीं जानता।
व्याख्या : तीन गुणों से भ्रमित जनगण भगवान् को नहीं जानते। उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण वे उसकी आराधना नहीं करते। किन्तु सर्वज्ञ होने के कारण भगवान् प्राणियों का भूत, वर्तमान और भविष्यकाल जानते हैं। अनन्यमनस्क भक्ति से भगवान् की पूजा करने वाला उसे तत्त्व रूप से जान लेता है। उसे परमात्मा की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान होता है।
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ।।२७ ।।
शब्दार्थ : इच्छाद्वेषसमुत्थेन-इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, द्वन्द्वमोहेन द्वन्द्वों के मोह के कारण, भारत- हे भारत, सर्वभूतानि-सभी प्राणी, संमोहम् - मोह को, सर्गे-जन्म-काल में, यान्ति-जाते हैं, परंतप-हे शत्रुओं के विजेता ।
अनुवाद : हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वन्द्वों के मोह वश संसार के समस्त प्राणी जन्म लेकर भ्रमित हो रहे हैं।
व्याख्या : जहाँ सुख है वहाँ राग है, आसक्ति है और जहाँ दुःख है वहाँ द्वेष है, विरक्ति है। शरीर के रक्षण की मनुष्य में स्वाभाविक प्रकृति होती है। मनुष्य उन साधनों को प्राप्त करना चाहता है जिनसे शरीर की रक्षा हो सकती है। शरीर और मन को पीड़ा पहुँचाने वाले पदार्थों से मनुष्य छुटकारा पाना चाहता है। द्वन्द्वों के कारण उत्पन्न मोह से इच्छा और द्वेष प्रस्फुटित होते हैं और मनुष्य उन पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । इन्द्रिय ग्राह्य बाह्य संसार का भी सच्चा अनुभव नहीं कर सकता। यह कहना अनिवार्य नहीं है कि इच्छा-द्वेष से आवृत बुद्धि वाले मनुष्य में अन्तस्तम आत्मा का आध्यात्मिक ज्ञान उदित नहीं हो सकता।
राग और द्वेष, सुख और दुःख, गर्मी और सर्दी, हर्ष और शोक, प्रसन्नता और पीड़ा, सफलता और विफलता, मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा विरोधी द्वन्द्वों के युग्म हैं। राग-द्वेष (अथवा आकर्षण विकर्षण) सभी प्राणियों में भ्रम (मोह) जागृत करते हैं और आत्म ज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश में बाधा डालते हैं।
जिसकी बुद्धि द्वन्द्वों से मोहित है वह यह अनुभूति नहीं कर सकता कि "मैं आत्मा हूँ", इसीलिए वह मुझे आत्म-रूप में नहीं देखता ।
राग-द्वेष का शिकार व्यक्ति विवेक शक्ति खो बैठता है। वह चाहता है कि सुखद पदार्थ तो सर्वदा सुलभ होते रहें और दुःखद पदार्थ अचिरेण लुप्त हो जाएं। यह कैसे सम्भव है ? देश, काल और कारणत्व में आबद्ध पदार्थ तो नष्ट होंगे ही। आज जो रुचिकर और अनुकूल है वह कुछ समयोपरान्त अरुचिकर और प्रतिकूल हो जाएगा। मन चंचल है। इसे विभिन्नता अथवा परिवर्तन चाहिए। एक ही प्रकार (एक रूपता) से यह उद्विग्न हो जाता है।
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ।।२८ ।।
शब्दार्थ : येषाम् - जिनका, तु-लेकिन, अन्तगतम् - अन्त की ओर (विनष्ट), पापम् -पाप, जनानाम् -मनुष्यों का, पुण्यकर्मणाम् -पुण्य कर्म करने वालों का, ते-वे, द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः - द्वन्द्वों के मोह से विमुक्त, भजन्ते-पूजा करते हैं, माम् -मेरी, दृढव्रताः दृढ़ व्रतधारी।
अनुवाद : परन्तु वे पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य जिनके पाप भस्मीभूत (विनष्ट) हो चुके हैं और जो राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों के मोह से मुक्त हो चुके हैं, वे कृतसंकल्प हो कर मेरी पूजा करते हैं।
व्याख्या : पुण्य कृत्यों से हृदय परिष्कृत होता है। सत्त्व की वृद्धि होती है। रजस् और तमस् धीरे-धीरे क्षीण होता है, मन सौम्य और शान्त होने लगता है। तुच्छ अहंयुक्त व्यक्तित्व शनैः-शनैः समाप्त होने लगता है। आध्यात्मिकता का विकास होता है। दिव्य आभा और अधिक कांति को प्राप्त होती है और तुम अकर्तृक (व्यक्तित्व शून्य) बन जाते हो।
पाप-परम सत्ता के साथ अभेदभाव को भूलना ही सब से बड़ा पाप है। भेद दर्शन पाप है। शरीर को ही आत्मा मान बैठना और संसार को सत्य मान लेना पाप है। अहंभाव में रहना पाप है। अज्ञान पाप है।
दृढ़व्रताः - दृढ़ व्रत वाला व्यक्ति अचल संकल्प वाला होता है। इस प्रकार का उसका संकल्प होता है-"मुझे आत्मसाक्षात्कार करना ही है। आत्म-ज्ञान प्राप्त किए बिना मैं अपने आसन से एक इंच भर भी नहीं हटूंगा।"
उसे पूर्ण विश्वास होता है कि "ब्रह्म ही सत्य है और जगत् मिथ्या है। यह संसार मृग-मरीचिका के समान है। मैं अमृतत्व और शाश्वत आनन्द की प्राप्ति कर सकता हूँ। आत्म-ज्ञान की प्राप्ति से ही यह सम्भव है। भौतिक पदार्थों में किंचित् मात्र भी सुख नहीं है।" अतः भगवान् कहते हैं-"दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति ही मेरी आराधना करते हैं।"
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ।।२९ ।।
शब्दार्थ : जरामरणमोक्षाय-वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, माम् -मुझे, आश्रित्य - (मेरी) शरण में आ कर, यतन्ति-यत्न करते हैं, ये जो, ते-वे, ब्रह्म-ब्रह्म को, तत्-उसे, विदुः - जानते हैं, कृत्स्नम् -समग्र, अध्यात्मम् -आत्म-ज्ञान, कर्म-कर्म, च-और, अखिलम्-सम्पूर्ण ।
अनुवाद : मेरी शरण में आ कर जो पुरुष जरा-मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास करते हैं वे पूर्ण रूप से उस ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को जान लेते हैं।
व्याख्या : वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सर्वोच्च भूमा को प्राप्त करते हैं जो स्वतन्त्र सत्ता हैं। उनके समस्त संशय पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। अब वे पूर्ण रूप से समझ लेते हैं कि सर्वस्व वासुदेव ही हैं। सर्वस्व ब्रह्म है, विभिन्नता अथवा अनेकता नहीं है।
उनका इस मर्त्य लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। और वे जरा-मृत्यु को जीत लेते हैं। वे अभी और यहीं मुक्त हो जाते हैं।
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।।३० ।।
शब्दार्थ : साधिभूताधिदैवम् - भौतिक जगत् और दैवी जगत् का स्वामी, माम् मुझ को, साधियज्ञम् यज्ञों का स्वामी, च-और, ये जो, विदुः जानते हैं, प्रयाणकाले मृत्यु के समय, अपि-भी, च-और, माम् -मुझे, ते-वे, विदुः - जानते हैं, युक्तचेतसः- युक्त चित्त वाले ।
अनुवाद : जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जानते हैं अर्थात् मुझे भौतिक जगत् (भूलोक), द्युलोक (देवलोक) और यज्ञलोक के स्वामी के रूप में जानते हैं, वे युक्तचित्त वाले लोग अन्तकाल में भी मेरा ध्यान प्राप्त करते हैं।
व्याख्या : वे जो दृढ़ संकल्प वाले हैं, मेरे शरणागत हैं, भूलोक में पंचभूतों के सिद्धान्त के ज्ञान रूप मुझे जानते हैं, द्युलोक में दैवी पक्षों के ज्ञान रूप मुझे जानते और यज्ञों के स्वामी के रूप में मुझे जानते हैं वे मृत्यु को नहीं प्राप्त होते। उनका स्मृति हास नहीं होता। संसार से विदा होते समय भी उनकी चेतना मुझ में लगी रहती है। इन तीनों रूपों में जो मेरी पूजा करता है अर्थात् संसार से प्रस्थान करते समय परमात्मा के सब रूपों को जानता है वह मुझे ही जानता है। (इस अध्याय को विज्ञान योग और ज्ञान योग भी कहते हैं।)
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ।।७ ।।
।। इति ज्ञानविज्ञानयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथाष्टमोऽध्यायः
अक्षरब्रह्मयोगः
अर्जुन उवाच
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ।।१ ।।
शब्दार्थ : किम् क्या, तत्-वह, ब्रह्म-ब्रह्म, किम् क्या, अध्यात्मम् - अध्यात्म, किम् -क्या, कर्म-कर्म, पुरुषोत्तम-पुरुषश्रेष्ठ, अधिभूतम् -अधिभूत, च-और, किम् -क्या, प्रोक्तम् -कहा गया है, अधिदैवम् अधिदैव, किम् -क्या, उच्यते-कहा गया है।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे पुरुष श्रेष्ठ, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव क्या है?
व्याख्या : सातवें अध्याय के अन्तिम दो श्लोकों में भगवान् कृष्ण ने अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन गुह्य दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया। अर्जुन को इन विशेष शब्दों के अर्थ का ज्ञान नहीं है इसीलिए वह उपरोक्त प्रश्नों की अर्थाभिव्यक्ति हेतु भगवान् से प्रार्थना करता है। भगवान् कृष्ण उन प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं।
इस अध्याय को 'अभ्यास योग' भी कहा जाता है क्योंकि इस अध्याय के श्लोक ७, ८, १०, १२, १३ और १४ आध्यात्मिक अभ्यास से सम्बद्ध हैं। श्लोक ७ में कर्म और भक्ति का समन्वित वर्णन है (हाथ मानवता और समाज की सेवा में और मन भगवान् की सेवा में समर्पित हो) । आठवां श्लोक अभ्यास योग से सम्बद्ध है। श्लोक १०, १२ और १३ में हठ योग का वर्णन है जिसमें यह बताया गया है कि आज्ञाचक्र, सहस्रार और ब्रह्मरन्ध्र में प्राणशक्ति का ऊर्ध्वारोहण कैसे हो । श्लोक १४ में सतत नाम स्मरण रूपी सहज योग का वर्णन है। केवल नाम जप से भी आध्यात्मिक साधक भगवान् को सहज ही प्राप्त हो सकता है।
ब्रह्म की प्रकृति, जीवात्मा (अध्यात्म), कर्म की प्रकृति, भौतिक जगत् की प्रकृति (अधिभूत), देदीप्यमान् देवों का ज्ञान (अधिदैव) और यज्ञ का रहस्य (अधियज्ञ), इस उपदेश में बताये गये हैं। पूर्ण तपस्वी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा। उसे न केवल इस अभिव्यक्त सृष्टि का ही ज्ञान होगा प्रत्युत् बुद्धि से परे ब्रह्म का भी ज्ञान होगा और सृष्टि की रचना क्यों हुई, इस का भी उत्तर प्राप्त होगा।
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ।।२ ।।
शब्दार्थ : अधियज्ञः अधियज्ञ, यज्ञों का अधिष्ठाता, कथम् -कैसे, कः-कौन, अत्र-यहाँ, देहे-शरीर में, अस्मिन्-इस (में), मधुसूदन-हे मधुसूदन, प्रयाणकाले-मृत्यु के समय, च-और, कथम् -कैसे, ज्ञेयः- जानने योग्य, असि-हो, नियतात्मभिः - जितेन्द्रिय द्वारा।
अनुवाद : हे मधु संहारक कृष्ण, इस देह में अधियज्ञ कौन और कैसे है? जितेन्द्रिय द्वारा अन्तकाल में आप किस प्रकार जाने जाते हो ?
व्याख्या : भगवान् से अर्जुन ने सात प्रश्न पूछे-
(१) ब्रह्म क्या है? क्या ब्रह्म उपाधि सहित है अथवा उपाधि रहित ? (२) यह इन्द्रियों का समूह है अथवा प्रत्यक् चैतन्य (Individual Consciousness) है, पृथक् है अथवा शुद्ध चैतन्य है ? (३) कर्म क्या है? क्या यज्ञ ही कर्म है? अथवा, यह यज्ञ से पृथक् है ? (४) अधिभूत, भूतों का ज्ञान है। यह पाँच तत्त्वों का ज्ञान है अथवा कुछ और है? (५) अधिदैव वह है जो देवताओं से सम्बद्ध है। यह देवताओं पर ध्यान है अथवा सूर्य मण्डल आदि से सम्बद्ध चेतना है? (६) अधियज्ञ वैदिक कर्मकाण्ड अथवा यज्ञों से सम्बद्ध है। यह पर-ब्रह्म (Supreme Being) है अथवा कोई देव विशेष है? यह तादात्म्य रूप है अथवा अभेद है? यह देह के भीतर वास करता है अथवा बाहर ? यदि यह देह के भीतर ही वास करता है तो यह बुद्धि है अथवा इससे पृथक् कुछ और? (७) अन्तकाल में जब स्मृति-हास हो जाता है, इन्द्रियाँ अपनी उष्णता खो बैठती हैं अर्थात् उनमें जीवन शक्ति नहीं रहती तब एकाग्रचित्त और संयतेन्द्रिय भगवान् को कैसे जान सकता है?
हे भगवान् मधुसूदन ! आप दयालु हैं। आपने मधु का वध कर के जनगण के दुःख दूर किये। अतः आप मेरी कठिनाइयाँ और सन्देह सहज रूप से दूर कर सकते हैं। हे सर्वज्ञ भगवन्! आपके लिए तो यह कुछ भी नहीं (इस कारण से अर्जुन भगवान् कृष्ण को मधुसूदन कह कर पुकार रहा है)।
श्री भगवानुवाच
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ।।३ ।।
शब्दार्थ : अक्षरम् - अक्षर (जिसका क्षय न हो), ब्रह्म-ब्रह्म, परमम् -परम, स्वभावः स्वभाव, अध्यात्मम् -आत्म-ज्ञानं, उच्यते-कहा जाता है, भूतभावोद्भवकरः -प्राणियों की उत्पत्ति और विकास का कारण, विसर्गः - आहुति (देवताओं को), कर्मसंज्ञितः-कर्म कहा जाता है।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : ब्रह्म अक्षर है, परम है। इसकी मूल प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों के अस्तित्व, अभिव्यक्ति और विकास के हेतु देवताओं के निमित्त किया गया त्यागरूप यज्ञ कर्म कहलाता है।
व्याख्या : ब्रह्म अक्षर है, अनश्वर है, अविकारी है, सनातन है, स्वयंभू है, स्व-प्रकाशित है, अव्यय और सर्वव्यापक है। समस्त पदार्थों का मूल स्रोत और गर्भ वही है। अभिव्यक्त सभी प्राणी उसी में वास करते हैं, गति करते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। इसीलिए वह परम है और अक्षर है।
इसकी मूल प्रकृति (स्वभाव) अध्यात्म है। ब्रह्मन् प्रत्येक व्यष्टि शरीर में अन्तरात्मा (प्रत्यगात्मा) रूप से निवसित है। वही अध्यात्म है। उपनिषद्
काल के एक महान् तपस्वी ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा- "हे गार्गी! भूलोक और द्युलोक अपने-अपने स्थान पर (निरालम्ब) खड़े हैं। ब्राह्मण इस ब्रह्म को अक्षर (अविनाशी) कहते हैं। न तो यह रक्त वर्ण है न श्वेत । न तो यह छाया है और न ही अन्धकार । न तो वायु है न आकाश। निराधार, गन्धहीन, अचक्षु, अश्रोत्र, अवाक्, अमनस्, अप्रकाश, श्वासरहित, अमुख, अपरिमित और इसके न भीतर कुछ है और न ही बाहर । न तो यह किसी का उपभोग करता है और न कोई इसका उपभोग करता है (न तो यह उपभोक्ता है और न ही उपभोज्य) ।" अक्षर तो केवल पर-ब्रह्म है।
अक्षर का अभिप्राय यहाँ पावन शब्द ॐ अथवा अव्यक्त से नहीं है। ॐ के लिए लय है। अव्यक्त प्रकृति का भी विनाश होता है। इसलिए ब्रह्म अक्षर है, अनश्वर है, परम पुरुष है। विराट् रूप है।
विसर्गः समस्त शुभ कर्म।
वह ऋत्विक् कर्म जिसमें देवताओं के लिए पकाये हुए भात आदि की आहुति दी जाती है और जो प्राणियों के उद्भव और विकास का कारण है, कर्म कहलाता है। यज्ञ में दी गई आहुतियाँ सूक्ष्म रूप धारण कर के सौर मण्डल में पहुँचती हैं। सूर्य से वर्षा होती है और विभिन्न प्रकार के अनाज, वनस्पतियाँ और फल अंकुरित होते हैं। जीवधारी (भूत) इन भोज्य पदार्थों और धान आदि पर निर्भर रहते हैं और पुष्ट होते हैं। इसलिए यज्ञ सब प्राणियों का उद्भव और आधार है।
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ।।४ ।।
शब्दार्थ : अधिभूतम् - अधिभूत, क्षरः- नश्वर, भावः- प्रकृति (स्वभाव), पुरुष: जीवात्मा, चऔर, अधिदैवतम्-अधिदैवत, अधियज्ञः अधियज्ञ, अहम् मैं, एव-ही, अत्र-यहाँ, देहे—शरीर में, देहभृताम् - देहधारियों में, वर-श्रेष्ठ ।
अनुवाद : हे नर श्रेष्ठ अर्जुन ! अधिभूत (तत्त्वों का ज्ञान) मेरी नश्वर प्रकृति है और पुरुष अथवा आत्मा अधिदैव है। इस शरीर में केवल मैं ही अधियज्ञ हूँ।
व्याख्या : अधिभूत नश्वर प्रकृति । समस्त विषयों सहित परिवर्तनशील पंचभौतिक जगत् अधिभूत हैं-सब भौतिक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु जिसका जन्म हुआ है और नाम-रूप का यह परिवर्तनशील जगत् अधिभूत ही है।
अधिदैव - 'पुरुष' का शाब्दिक अर्थ है- "वह जिससे प्रत्येक वस्तु भर जाती है" (पुर्-भरना) । इसका अभिप्राय यह भी है-"जो शरीर में रहता है" (पुरि शेते इति पुरुषः) । यह हिरण्यगर्भ, समष्टि-आत्मा अथवा पोषण कर्ता ही है जिससे सब प्राणी शक्ति ग्रहण करते हैं। यह साक्षी चेतना है।
अधियज्ञ-चेतना, यज्ञ का अधिष्ठातृ देवता । समस्त यज्ञों और कर्मों के स्वामी भगवान् विष्णु हैं। विष्णु सब यज्ञों से स्वयं को एकरूप कर लेते हैं। "यज्ञो वै विष्णुः", यज्ञ ही विष्णु है, वेद की तैत्तिरीय संहिता में ऐसा कथन है। भगवान् कृष्ण कहते हैं—“शरीर में समस्त याज्ञिक प्रक्रियाओं का मैं अधिष्ठातृ देव हूँ।" समस्त यज्ञ शरीर द्वारा होते हैं अतः कह सकते हैं कि वे शरीर में ही वास करते हैं।
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।।५ ।।
शब्दार्थ : अन्तकाले -मृत्यु के समय, च-और, माम् -मुझे, एव-ही, स्मरन्-स्मरण करता हुआ, मुक्त्वा-त्याग कर, कलेवरम् - शरीर को, यः-जो, प्रयाति-जाता है, सः- वह, मद्भावम् - मेरे भाव को, याति-प्राप्त करता है, नास्ति नहीं है, अत्र-यहाँ, संशयः सन्देह ।
अनुवाद : और जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय शरीर त्याग करते हुए केवल मेरा ही स्मरण करता है, वह मेरे ही भाव (स्वरूप) को प्राप्त होता है इसमें कोई सन्देह नहीं।
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।।६ ।।
शब्दार्थ : यम् -जिस, यम्-जिस, वा-अथवा, अपि-भी, स्मरन् समरण करता हुआ, भावम् -प्रकृति (विषय भाव), त्यजति-त्यागता है, अन्ते-अन्तिम समय में, कलेवरम् - शरीर, तम् -उस, एव -ही, एति-प्राप्त करता है, कौन्तेय हे कौन्तेय, सदा-सदा (सतत), तद्भावभावितः उस विषय का चिन्तन करते हुए।
अनुवाद : हे अर्जुन ! जिस-जिस भाव का चिन्तन करते हुए अन्तकाल में मनुष्य शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित (संलग्न) रहा है।
व्याख्या : अगले जन्म का निर्णय अन्तिम चिन्तन से होता है। जीवन का सर्वाधिक समुन्नत विचार मृत्यु काल में मन को आ घेरता है। और यह महत्वपूर्ण विचार वही होगा जिसने सामान्य जीवन काल में मानव-मन को आकृष्ट किया हो। अन्तिम विचार से ही पुनर्जन्म के नव शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। जैसे मनुष्य सोचेगा वैसा ही बनेगा। पूर्व-अभ्यास द्वारा सृजित संस्कारों की शक्ति अन्तकाल में स्मृति का कारण बनती है। जीवन भर जिन्होंने भगवत्-पूजा का अभ्यास किया है वे ही अन्तकाल में अपने इष्टदेव का स्मरण कर सकते हैं।
भ्रमर-कीट-न्याय की उपमा यहाँ चरितार्थ होती है। कीट सतत भ्रमर का ध्यान करता रहता है और अन्ततः तद्रूप हो जाता है। इसी प्रकार सतत इष्टदेव का स्मरण करते हुए मनुष्य उस देव से तद्रूप हो जाता है। नन्दिकेश्वर का दृष्टशन्त हमारे समक्ष है। उसने सतत भगवान् का स्मरण करते-करते वही स्वरूप प्राप्त कर लिया।
जीवनकाल में यदि तुम अनवरत रूप से अमर आत्मा का चिन्तन करते रहोगे तो अन्तिम समय में केवल आत्मा का विचार तुम्हारे मन में आयेगा और तुम अमरत्व प्राप्त करोगे। यदि हर समय शरीर का ही चिन्तन करते रहोगे और नश्वर शरीर से एकरूप रहोगे तो पुनः- पुनः जन्म लेना पड़ेगा । अन्तकाल में यदि श्वान (कुत्ता) का स्मरण करोगे तो वही जन्म लेना पड़ेगा । राजा भरत ने मृत्यु के समय अपने प्रिय हिरण का चिन्तन किया, उन्हें हिरण का ही शरीर मृत्यूपरान्त धारण करना पड़ा।
प्रत्येक मनुष्य का जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण होता है, निश्चित अभीप्साएँ (तृष्णाएँ), इच्छाएँ और आशाएँ होती हैं। उसका एक निश्चित चरित्र, स्वभाव, स्वाद, मनोवृत्ति और व्यवहार होता है यह सब उसके अवचेतन मन के संस्कारों वश है जो उसके अभिन्न अङ्ग बन चुके हैं। उसके अनुभवों की अमिट छाप का ही यह परिणाम है।
ऐसा मनुष्य सदा अपने शरीर और शारीरिक आवश्यकताओं का ही चिन्तन करता है। बाह्य नश्वर पदार्थों में वह सुख की खोज करता है। शरीर के साथ वह तादात्म्य स्थापित कर लेता है। सब पदार्थों के स्रोत अन्तस्तम आनन्दमय शाश्वत आत्मा की तो वह उपेक्षा करता है। भौतिक जगत् की खोज के लिए वह अपने शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धि को प्रशिक्षित करता है। वह मन और इन्द्रियों के यौगिक अनुशासन की उपेक्षा करता है। इसलिए वह सदा अपने शरीर, भोजन, पानी और वस्त्र की चिन्ता में लगा रहता है। सुख और ज्ञान के आलोकपुञ्ज भीतर विद्यमान अपने आत्मा और परमात्मा को वह भूला रहता है।
इच्छाएँ अनन्त हैं। एक जन्म में उनकी पूर्ति असम्भव है। अन्त समय में संचित इच्छाओं और संस्कारों के भण्डार का मन्थन होता है। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रबल और हृदयग्राही इच्छा मानस पटल पर आ जाती है। यह मन्थन की हुई हार्दिक इच्छा तत्काल सन्तुष्टि हेतु मनुष्य का ध्यान आकृष्ट करती है और मृत्यु के समय वह उसी का विचार करता है। जिस प्रकार एक जीवन्त आम का पौधा नर्सरी में भली प्रकार विकसित होता है उसी प्रकार प्रबलतम इच्छा मानस पटल पर अंकुरित हो उठती है। इच्छा पूर्ण न होने पर प्रबल रूप से मन पर छा जाती है और अगले जन्म में इसकी पूर्ति होती है। यही इच्छा आगामी जन्म में अत्यधिक प्रबल होगी।
तुम स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता (भाग्य को लिखने वाले) हो। अपने अनुभवों, भावों, चरित्र और विचारों के लिए तुम स्वयं ही उत्तरदायी हो। तुमने ही अपने अवचेतन मन में सांसारिक इच्छाओं और संस्कारों के बीज बोये हैं और उन्हें अंकुरित और विकसित होने का अवसर दिया है। आध्यात्मिक संस्कार के यदि तुमने बीज बोये होते हो अमृतत्व और शाश्वत आनन्द की फसल काटते। जैसा बोओगे, वैसा काटोगे।
जीवन भर, आत्मा अथवा इष्टदेव पर सतत चिन्तन करने वाला मनुष्य अविचलित मन से मृत्यु का सामना करेगा। वही अन्त समय में सच्चिदानन्द परमात्मा का ध्यान करता हुआ संसार से विदा हो कर उस परमात्मा को प्राप्त होगा। ईश्वर के प्रति अनन्य भक्तिभाव होना चाहिए। तुम्हारा समग्र चित्त उसी में लीन हो। स्वार्थ भाव से पूर्ण किसी भी इच्छा को अवचेतन मन में स्थान मत दो। तभी मृत्युकाल में भगवान् का चिन्तन कर सकोगे और उनके भाव को प्राप्त करोगे।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ।।७।।
शब्दार्थ : तस्मात् - इसलिए, सर्वेषु-सब, कालेषु-कालों में, माम् मुझे, अनुस्मर स्मरण करो, युध्य-युद्ध करो, च-और, मय्यर्पितमनोबुद्धिः मन और बुद्धि मुझ में एकाग्रित कर के (समर्पित कर के), माम् -मुझे, एव-केवल, एष्यसि आओगे (मुझे प्राप्त करोगे), असंशयम् - निस्सन्देह ।
अनुवाद : इसलिए समस्त कालों में मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो । मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर के तुम निस्सन्देह मुझे ही प्राप्त करोगे ।
व्याख्या : अनन्यभाव से मन भगवान् के चरणों में संलग्न हो। मन और बुद्धि उसमें लगा कर कर्म करो।
युध्य-अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। इससे हृदय परिमार्जित होगा, ज्ञान का उदय होगा और तुम मेरे पास आओगे। 'युद्ध' शब्द उपलक्षणा (उपदेशात्मक) भाव में प्रयुक्त हुआ है। इसका अभिप्राय है-“अपने वर्णाश्रम के अनुसार निज कर्तव्य का पालन करो।" वर्णाश्रम धर्म में विभिन्न वर्ण और जीवन की अवस्था के अनुरूप कर्त्तव्य और नित्य-नैमित्तिक कर्म में अनुष्ठान के नियमों का संकेत है। (विवरण-V.13)
ध्यान के विषय स्वरूप में चित्त-वृत्ति भावना कहलाती है (मानसिक नियमन अथवा रूपान्तरण, चित्तवृत्ति है)। सगुण उपासना का अभ्यास करने वालों के लिए भावना है। आत्मनिष्ठ ज्ञानी के लिए प्रयाणकाल (मृत्यु के समय) में भावना अनिवार्य नहीं है। (निरूपण - IX.34; XII.8,11)
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ।।८ ।।
शब्दार्थ : अभ्यासयोगयुक्तेन-(ध्यान के) अभ्यास रूपी योग से युक्त, चेतसा-मन से, न -नहीं, अन्यगामिना-अन्यत्र गति वाला, परमम् परम, पुरुषम् -पुरुष को, दिव्यम् -दिव्य, याति प्राप्त होता है, पार्थ हे पार्थ, अनुचिन्तयन् -चिन्तन करता हुआ।
अनुवाद : हे पार्थ, जिसका मन अभ्यास रूपी योग से युक्त हो, अन्यत्र न भटकता हो और सदा परमात्मा का चिन्तन करने वाला हो ऐसा मनुष्य उस देदीप्यमान ज्योतिर्मय परम पुरुष को प्राप्त होता है।
व्याख्या : अभ्यास-ईश्वर की एक ही विचारधारा का सतत चिन्तन अभ्यास है। ध्यान के अभ्यास में विजातीय वृत्तियों (सांसारिक विचार अथवा ध्यान के विषय से पृथक् विचार) का शमन कर के सजातीय वृत्ति प्रवाह होता है अर्थात् केवल परमेश्वर के गुणों की विचारधारा प्रवाहित होती है। यही अभ्यास है। अभ्यास ही योग है। निर्विकल्प समाधि में इसका उपराम हो जाता है। समाहित चित्त वाला योगी परमात्मा को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से नदियाँ अपना नाम और रूप त्याग कर सागर के साथ एकरूप हो जाती हैं उसी प्रकार ज्ञानी अपने नाम और रूप से मुक्त हो कर, शुभाशुभ से ऊपर उठ कर परमात्मा के साथ तादात्म्यता प्राप्त कर लेता है।
इस अभ्यास में नियमितता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य है। ध्यान में नियम का पालन करो। अचिरेण लक्ष्य प्राप्ति करोगे।
पुरुषं दिव्यम् - देदीप्यमान देहातीत अन्तर्यामी पुरुष जो सौर मण्डल में विद्यमान है।
गुरु के आदेशों का पालन करते हुए शास्त्र-विहित कर्म करते हुए, मन को विषय-वासनाओं से पराङ्मुख कर के जो मनुष्य सतत ध्यान का अभ्यास करता है वह परम पुरुष को प्राप्त करता है।
कविं पुराणमनुशासितार-
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।।९ ।।
शब्दार्थ : कविम् सर्वज्ञ (क्रान्तदर्शी), पुराणम् -सनातन, अनुशासितारम् -शासक (सम्पूर्ण जगत् का), अणोः - अणु से, अणीयांसम् -सूक्ष्मतर, अनुस्मरेत् -स्मरण करता है, यः-जो, सर्वस्य-सब का, धातारम् -पालनकर्ता को, अचिन्त्यरूपम् -चिन्तन से परे है जिसका स्वरूप, आदित्यवर्णम् -सूर्य की भाँति प्रकाशमान, तमसः- (अज्ञान रूप) अन्धकार से, परस्तात् - परे ।
अनुवाद : सर्वज्ञ, सनातन, विश्व के शासक, अणु से भी सूक्ष्मतर, सब के पालनकर्ता, अचिन्त्य, अज्ञान-अन्धकार से परे सूर्य की भाँति देदीप्यमान का जो भी ध्यान करता है-
व्याख्या : कविम् ज्ञानी, द्रष्टा, कवि, सर्वज्ञ।
भगवान् जीवों को उनका कर्म-फल प्रदान करता है। वह जगत् का स्वामी है, शासक है, नियन्ता है। उसके स्वरूप का ध्यान अतीव दुष्कर कार्य है। वह अपनी ही ज्योति से ज्योतित (स्वयं प्रकाश) है। वह सूर्य की भाँति प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करता है।
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।
ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।।१० ।।
शब्दार्थ : प्रयाणकाले -मृत्यु के समय, मनसा-मन से, अचलेन-निश्चल, भक्त्या-भक्ति भाव से, युक्तः -युक्त, योगबलेन-योगबल से, च-और, एव-केवल, ध्रुवोः-दो भौहों के, मध्ये-मध्य में, प्राणम् - प्राण (श्वास), आवेश्य-स्थापित कर के, सम्यक्-अच्छी प्रकार, सः- वह, तम्-उस, परम् -परम, पुरुषम् -पुरुष को, उपैति -पहुँचता है, दिव्यम् - दिव्य ।
अनुवाद : अन्तकाल में, निश्चल मन से, भक्तिभाव से पूर्ण हो कर, योग की शक्ति से श्वास को दोनों भृकुटियों के मध्य स्थित कर के जो प्रयाण करता है वह उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है।
व्याख्या : योगी के पास असीम आन्तरिक बल और एकाग्रता की शक्ति होती है। धारणा और ध्यान के अनवरत अभ्यास से उसका चित्त पूर्णतया स्थिर हो जाता है। पहले वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों पर ध्यान का अभ्यास करता है। तत्पश्चात् वह अनाहत चक्र (हृदय कमल) पर ध्यान करता है। तदनन्तर प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी से लाकर भ्रूमध्य आज्ञा चक्र पर स्थिर करता है। इस योगाभ्यास से वह अनायास ही परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है।
जीवन भर योग के अभ्यास में समर्पित व्यक्ति के लिए ही यह सम्भव है।
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।।११ ।।
शब्दार्थ : यत्-जो, जिस, अक्षरम्-अविनाशी, वेदविदः- वेदज्ञ (वेद को जानने वाले), बदन्ति-कहते हैं, विशन्ति-प्रवेश करते हैं, यत्-जो, यतयः-संन्यासी (जितेन्द्रिय), वीतरागाः-अनासक्त, यत्-जो, इच्छन्तः - इच्छा करते हुए, ब्रह्मचर्यम् ब्रह्मचर्य, चरन्ति-अभ्यास करते हैं, तत्-उस, ते तुम्हें, पदम् लक्ष्य को, संग्रहेण-संक्षेप से, प्रवक्ष्ये-कहूँगा।
अनुवाद : मैं उस परम पद को तेरे लिए कहूँगा जिसे वेदों के ज्ञाता अविनाशी कहते हैं, विरक्त और जितेन्द्रिय संन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है।
व्याख्या : परम पुरुष प्रतीकात्मक रूप से प्रणव अथवा पावन एकाक्षर शब्द ॐ से अभिहित है। यह मनुष्य का परम लक्ष्य अथवा सर्वोच्च पद है।
यही विचारधारा कठोपनिषद् में अभिव्यक्त की गई है। यम (मृत्यु के देवता) ने नचिकेता से कहा - "समस्त वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त प्रकार के तप जिसकी घोषणा करते हैं और जिसकी कामना करते हुए वे (तपस्वी, यति) ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करते हैं वह पद मैं तुम्हें संक्षेप में कहूँगा। वह है ॐ (ओ३म्)"। शिबि के पुत्र सत्यकाम ने पिप्पलाद से प्रश्न किया- 'हे भगवन्, मनुष्य में यदि कोई जीवन-पर्यन्त (मृत्यु के समय तक) ॐ का ध्यान करे तो उसे कौन सा लोक प्राप्त होगा?' पिप्पलाद ने कहा- 'हे सत्यकाम, अक्षर 3 deg ही उच्च व निम्न ब्रह्म है। जो मनुष्य उच्चतर पुरुष पर तीन मात्रा वाले अक्षर ॐ (ओ३म्) का ध्यान करता है उसे सामवेद की ऋचायें ब्रह्मलोक में ले जाती हैं।' (प्रश्नोपनिषद्) ।
प्रणव अथवा ॐ परम पुरुष की अभिव्यक्ति अथवा मूर्त रूप (प्रतीक) माना जाता है यह मूढ़ मन्द बुद्धि मनुष्यों को भी साक्षात्कार कराने में सहायक है।
ध्यान के प्रारम्भ में तीन बार ॐ का उच्चारण करो। सहज ही मन एकाग्र होगा।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ।।१२ ।।
शब्दार्थ : सर्वद्वाराणि समस्त द्वार, संयम्य-वश में कर के, मन:-मन, हृदि-हृदय में, निरुध्य स्थिर कर के, च-और, मूर्ति-मस्तक में, आधाय-स्थापित कर के, आत्मनः-अपने, प्राणम् -प्राणों को, आस्थितः - स्थिर कर के, योगधारणाम् - योग धारणा को।
अनुवाद : समस्त द्वार बन्द कर के, मन को हृदय में नियुक्त कर के और प्राण शक्ति को मस्तक में स्थिर कर के धारणा के अभ्यास में संलग्न,
व्याख्या : ज्ञानेन्द्रियाँ द्वार हैं। द्वार बन्द करने का अभिप्राय है- प्रत्याहार के अभ्यास से इन्द्रियों का वशीकरण । इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाना प्रत्याहार है। इन्द्रियाँ संयत हो भी जायें तो भी मन ऐन्द्रिक विषयों में विचरण करता रहेगा। इसलिए मन को हृदय-कमल में एकाग्रित (स्थिर) करना है जिससे सारे विचार और मनोवृत्तियाँ नियन्त्रित हो जायें। अब संपूर्ण प्राण को ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर किया जाता है।
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ।।१३।।
शब्दार्थ : ॐ -ॐ, इति-इस प्रकार, एकाक्षरम् - एक अक्षर वाला, ब्रह्म-ब्रह्म, व्याहरन्-उच्चारण करते हुए, माम् -मुझे, अनुस्मरन् स्मरण करते हुए, यः-जो, प्रयाति-जाता है, त्यजन्-त्यागते हुए, देहम् - शरीर को, सः वह, याति-प्राप्त करता है, परमाम् -परम, गतिम् लक्ष्य को ।
अनुवाद : ब्रह्म-स्वरूप एकाक्षर ॐ का उच्चारण करते हुए और मेरा चिन्तन करते हुए जो मनुष्य प्राण-त्याग करता है वह परम पद को प्राप्त करता है।
व्याख्या : योगी अपने विचारों को नियन्त्रित कर के, हृदय से ऊर्ध्वगमन करने वाली सुषुम्ना नाड़ी hat H (प्राणों का) आरोहण करता है। वह अपने समस्त प्राण ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर कर लेता है। वह पावन एकाक्षर का उच्चारण करता है, मेरा ध्यान करता है और देह-त्याग कर देता है।
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।।१४ ।।
शब्दार्थ : अनन्यचेताः- जब मन किसी अन्य विषय का चिन्तन न करे, सततम् निरन्तर, यः-जो, माम् -मुझे, स्मरति स्मरण करता है, नित्यशः-नित्य, तस्य-उसके (लिए), अहम् -मैं, सुलभः सहज ही प्राप्य, पार्थ-हे पार्थ, नित्ययुक्तस्य-सदायुक्त, योगिनः- योगी को ।
अनुवाद : हे पार्थ, (चिरकाल तक) अनवरत रूप से नित्य अनन्यमनस्क (एकाग्रचित्त) भाव से मेरा चिन्तन करने वाले नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ (सहज प्राप्य) हूँ।
व्याख्या : जीवनपर्यन्त भगवान् का सतत चिन्तन उनकी प्राप्ति का सहज उपाय है।
अनन्यचेताः-किसी अन्य विषय की ओर साधक का ध्यान न हो। इष्ट देव के अतिरिक्त वह अन्य का ध्यान न करे।
नित्यशः - दीर्घावधि पर्यन्त अर्थात् जीवनपर्यन्त ।
जो मनुष्य भगवान् का ध्यान प्रारम्भ कर के बीच में छोड़ देता है, छः मास तक स्मरण करता है फिर अभ्यास छोड़ देता है और इस प्रकार पुनः-पुनः अभ्यास का प्रारम्भ और त्याग करता है वह भगवान् को नहीं पा सकता। (मिरूपण-IX.22, 34)
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।। १५ ।।
शब्दार्थ : माम् -मुझ को, उपेत्य-प्राप्त कर के, पुनर्जन्म पुनः जन्म, दुःखालयम् दुःख का घर, अशाश्वतम् - अनित्य, न-नहीं, आप्नुवन्ति-प्राप्त करते हैं, महात्मानः- महात्मा लोग, संसिद्धिम् -सिद्धि को, परमाम् -परम, गताः-पहुँच कर।
अनुवाद : मुझे प्राप्त होने के उपरान्त महात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते जो क्षणिक है और दुःख का घर है। वे पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं।
व्याख्या : जन्म, शरीर से उत्पन्न होने वाले दुःखों का घर है। गर्मोपनिषद् का अध्ययन करो। किस प्रकार शिशु गर्भ में कैद होता है, योनि मार्ग में और गर्भाशय के मुख में धकेला जाता है। इसके पश्चात् प्रसूति-वायु से प्रभावित होता है जो शिशु को जन्म देने में सहायक है।
महात्मा-महान् आत्माएँ। ये रजस् और तमस् से मुक्त होते हैं।
मामुपेत्य-यह क्रम-मुक्ति का संकेत है। उपासना की शक्ति से देवयान (मार्ग) से जाने वाले ब्रह्मलोक (सृष्टिकर्ता का लोक) अथवा सत्यलोक (जो सात लोकों में सर्वोच्च है) को प्राप्त करते हैं और वहाँ वे दैवी सम्पदा और भगवान् की महिमा का आनन्द लेते हुए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कैवल्य मोक्ष (अन्तिम मोक्ष) को प्राप्त करते हैं और ब्रह्माण्ड के प्रलय काल में ब्रह्मा का सान्निध्य प्राप्त करते हैं। मुक्त आत्माएँ पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करतीं। जो मुझे प्राप्त नहीं करते वे पुनः-पुनः संसार में आते हैं।
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।।१६ ।।
शब्दार्थ : आब्रह्मभुवनात् - ब्रह्मलोक पर्यन्त, लोकाः- लोक, पुनरावर्तिनः पुनरावर्ती (पुनः आने वाले), अर्जुन-हे अर्जुन, माम् -मुझे, उपेत्य- प्राप्त कर के, तु-लेकिन, कौन्तेय-हे कौन्तेय, पुनर्जन्म पुनः जन्म, न-नहीं, विद्यते-होता ।
अनुवाद : हे अर्जुन, ब्रह्म लोक सहित समस्त लोक पुनरावर्ती हैं परन्तु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या : वे भक्त जो दहरोपासना (हृदय के गुह्य आकाश में एक
प्रकार की गहन उपासना) का अभ्यास करते हैं और अन्य भक्त जो देवयान (देवमार्ग) से ब्रह्मलोक को पहुँच कर क्रम-मुक्ति प्राप्त करते हैं वे इस लोक में पुनः नहीं लौटते ।
किन्तु जो भक्त पञ्चाग्नि विद्या के अभ्यास से ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे वे ब्रह्मलोक में पुण्य कर्मों का फल भोग कर भूलोक में पुनः अवतरित होंगे। समस्त लोक काल-बद्ध हैं अर्थात् काल की सीमा में सीमित हैं अतः उन लोकों से पुनः नीचे भूलोक पर आना पड़ता है। (केवल परमात्मा कालातीत है।)
सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः ।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।।१७ ।।
शब्दार्थ : सहस्रयुगपर्यन्तम् -सहस्र युग पर्यन्त, अहः-दिन, यत्-जो, ब्रह्मणः ब्रह्म के, विदुः जानते हैं, रात्रिम् -रात्रि को, युगसहस्रान्ताम् -सहस्र युग में समाप्त होने वाली,ते -वे , अहोरात्रविदः- रात्रि और दिवस के ज्ञाता है, जनाः लोग ।
अनुवाद : ब्रह्मा के एक सहस्र युग वाले दिवस और एक सहस्र युग वाली रात्रि को जो योगी जानते हैं वे ही वस्तुतः दिवस और रात्रि को जानते हैं।
व्याख्या : दिवस का अभिप्राय है-सृष्टि का उद्भव, प्रसार अथवा अभिव्यक्ति। रात्रि का अभिप्राय है सृष्टि की प्रलय । समस्त लोक काल की अवधि में आबद्ध हैं, सीमित हैं। अतः वे पुनः लौटते हैं। ब्रह्म लोक भी अनित्य है यद्यपि इसकी अवधि सहस्र युग है। जब चार महान् युग एक सहस्र बार व्यतीत होते हैं तो यह ब्रह्मा का एक दिवस कहलाता है और जब इतने ही युग अर्थात् चार महान युग एक सहस्र बार पुनः व्यतीत होते हैं तो यह ब्रह्मा की एक रात्रि कही जाती है। जो इस दिवस और रात्रि पर्यन्त रह सकते हैं और इसके द्रष्टश बन सकते हैं वे ही दिवस और रात्रि का ज्ञान रखते हैं।
सूर्य सिद्धान्त इसी काल-विभाग का निरूपण करता है।
इस सिद्धान्त के अनुसार-
कलियुग (संध्या और संध्यांश सहित) ४,३२,००० वर्ष
द्वापर युग. ८,६४,००० वर्ष
त्रेतायुग. १२,९६,००० वर्ष
कृतयुग. १७,२८,००० वर्ष
इस प्रकार एक महायुग चार युगों
के समनुरूप है ४३,२०,००० वर्ष
सांध्य योग सहित ७१ ऐसे महायुगों से
१७,२८,००० वर्षों के अन्त में एक मन्वन्तर
बनता है जिसकी अवधि है ३०,८४,४८,००० वर्ष
एक और संध्या सहित १४ ऐसे मन्वन्तरों
के योग से १७,२८,००० वर्षों के अन्त में
एक कल्प बनता है। उसकी अवधि है. ४,३२,००,००,००० वर्ष
दो कल्प से ब्रह्मा का एक दिवस और
रात्रि बनते हैं। अवधि है ८,६४,००,००,००० वर्ष
३६० ऐसे दिन और रात से ब्रह्मा का
एक वर्ष बनता है जिसकी अवधि है. ३१,१०,४०,००,००,००० वर्ष
१०० ऐसे वर्ष ब्रह्मा का जीवन काल हैं
जिसकी अवधि है ३१,१०,४०,००,००,००,००० वर्ष
सृष्टि की प्रलय के समय विश्व अव्यक्त अथवा मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। जिस प्रकार एक वृक्ष बीज में अव्यक्तावस्था में पड़ा रहता है उसी प्रकार प्रलय काल में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मूल प्रकृति में बीज रूप से अव्यक्तावस्था में रहता है। यह ब्रह्मा की रात्रि है। यह ब्रह्माण्डीय रात्रि है।
पुनः महाकल्प (उत्पत्ति) के समय सृष्टि का विस्तार होता है। ब्रह्माण्डीय दिवस का यह उषाकाल है। वैश्विक दिवस के लय-विलय का क्रम इस बृहत् ब्रह्माण्ड में चलता रहता है।
इस ब्रह्माण्डीय दिवस और रात्रि रूपी नित्यवर्ती (नित्य घूमने वाले) चक्र में आने वाली कोई भी वस्तु नित्य रहने वाली नहीं है। इसी कारण से उपनिषदों के द्रष्टा (ऋषि), पुरातन ऋषियों ने इस वैश्विक अहोरात्र से परे अलौकिक परम पुरुष में वास किया जो अमर आत्मा है, अनिर्वचनीय पुरुष है, जीवन का परम लक्ष्य है, मनुष्य का सर्वोच्च ध्येय (अवसान) है। दग्ध बीज जिस प्रकार अंकुरित नहीं होते उसी प्रकार जिन्होंने उस शाश्वत, अविनाशी परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है वे दुःख, कष्ट और पीड़ा से भरे इस संसार में पुनः नहीं लौटते। उन्हें न तो दिवस का ध्यान है और न ही रात्रि का। वे सच्चिदानन्द स्वरूप के साथ एक हो गए हैं।
व्यक्त और अव्यक्त दोनों का वास ब्रह्म में है। ब्रह्म इन दोनों से अतीत है। जब संसार और शरीर नष्ट हो जाते हैं तब भी ब्रह्म की सत्ता विद्यमान रहती है। सागर में लहरें उठती हैं और शान्त हो जाती हैं किन्तु सागर अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार सृष्टियाँ बनती हैं और नष्ट होती हैं किन्तु सब वस्तुओं का और मूल प्रकृति का स्रोत ब्रह्म अप्रभावित रहता है।
स्वर्ण आभूषण जैसे स्वर्ण से बनते हैं और पिघलाने पर स्वर्ण में लीन हो जाते हैं इसी भाँति सभी लोकों का ब्रह्म से उद्भव होता है और ब्रह्म में ही लय होता है। कुण्डल, कंगन, नूपुर (पायल) आदि विभिन्न स्वरूपों से स्वर्ण प्रभावित नहीं होता । इसी प्रकार सृष्टि के लय-विलय से और शरीरों के विनाश से ब्रह्म प्रभावित नहीं होता। वह सदा एक रस रहता है।
अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ।।१८ ।।
शब्दार्थ : अव्यक्तात् अव्यक्त से, व्यक्तयः व्यक्त, सर्वाः-सब, प्रभवन्ति-उत्पन्न होते हैं, अहरागमे - दिवस के प्रारम्भ में, रात्र्यागमे-रात्रि आने पर, प्रलीयन्ते-लीन हो जाते हैं, तत्र-वहाँ, एव-ही, अव्यक्तसंज्ञके-अव्यक्त में।
अनुवाद : दिवस के प्रारम्भ में अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि का उद्भव होता है और रात्रि होने पर समस्त सृष्टि निश्चित रूप से केवल उसी में लीन हो जाती है जिसे अव्यक्त की संज्ञा दी गई है।
व्याख्या : ब्रह्माण्डीय दिवस के प्रारम्भ में ब्रह्मा के जागने पर समस्त चराचर जगत् (जड़ और चेतन), अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्माण्डीय रात्रिकाल में जब ब्रह्मा सोते हैं तब सभी अभिव्यक्त सृष्टि अव्यक्त में विलीन हो जाती है।
अहरागमः-सृष्टि का प्रारम्भ
रात्र्यागमः - प्रलय का प्रारम्भ - (निरूपण -IX.7,8 )
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ।।१९ ।।
शब्दार्थ : भूतग्रामः -प्राणी समुदाय, सः- वह, एव-निश्चित रूप से, अयम् -यह, भूत्वा भूत्वा पुनः-पुनः जन्म ले कर, प्रलीयते-विलीन हो जाता है, रात्र्यागमे-रात्रि आने पर, अवशः-असहाय, पार्थ-हे पार्थ, प्रभवति उत्पन्न होता है, अहरागमे-प्रातः होने पर (दिवस के प्रारम्भ में)।
अनुवाद : हे अर्जुन, वही प्राणी समुदाय परवश हुआ बारम्बार जन्म लेकर (अव्यक्त में) ब्रह्मा की रात्रि के प्रारम्भकाल में विलीन हो जाता है और दिवस के प्रारम्भ काल में पुनः उत्पन्न होता है।
व्याख्या : अविद्या (अज्ञान), काम (इच्छा) और कर्म की ये तीन ग्रंथियाँ मनुष्य को संसार के बन्धन में डालने वाली हैं। इच्छा अज्ञान से उत्पन्न होती है। अभीप्सित (इच्छित) पदार्थों को प्राप्त करने के लिए और उनका उपभोग करने के लिए मानव संघर्ष करता है। इस क्रिया-कलाप में राग-द्वेष, प्रेम-घृणा और आकर्षण-विकर्षण के वशीभूत हो कर वह किसी का तो अनुमोदन करता है और किसी को चोट पहुँचाता है। अतः वह आवागमन के चक्र में फंस जाता है। अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए उसे पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। निज कर्मों के बल से ही वह पुनः पुनः आता-जाता रहता है।
अज्ञान, काम और कर्म के बन्धन में आ कर व्यष्टि आत्माओं ने स्वतन्त्रता खो दी है। इसलिए उन्हें इस संसार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उनके मन में अनासक्ति उत्पन्न करने के लिए और उनके हृदय में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न करने के लिए तथा यह अन्धविश्वास मिटाने के लिए कि मनुष्य अपने कर्मों का फल नहीं भोगता अथवा यह सोचना कि जो कर्म उसने नहीं किया उसका फल भोगता है-भगवान् ने कहा है कि सभी जीव पर वश हुए दिवस के प्रारम्भ में बारम्बार जन्म लेते हैं और रात्रिकाल प्रारम्भ होने पर प्रलय में विलीन हो जाते हैं। इन सब का कारण है अज्ञान वश इच्छा का उद्भव और इच्छापूर्ति हेतु कर्म करना और फिर परिणाम भोगना ।
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।। २० ।।
शब्दार्थ : पर:-उच्चतर, तस्मात् - उस से, तु-लेकिन, अन्यः-अन्य, अव्यक्तः - अव्यक्त, अव्यक्तात् - अव्यक्त से, भावः सत्ता, सनातनः -शाश्वत, यः-जो, सः-वह, सर्वेषु सब (में), भूतेषु-प्राणियों में, नश्यत्सु नष्ट हुए, न-नहीं, विनश्यति नष्ट होता।
अनुवाद : परन्तु निश्चित रूप से इस अव्यक्त से भी परे एक और उच्चतर अव्यक्त की सत्ता है जो शाश्वत है, सनातन है और सब जीवों के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती।
व्याख्या : अव्यक्त का अन्य अस्तित्व सनातन, शाश्वत पर ब्रह्म का है जो मूल प्रकृति अथवा अव्यक्त से पृथक् है। उसकी प्रकृति सर्वथा भिन्न है। वह हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठतर है जो वैश्विक सृजनात्मक प्रज्ञा है। मूल प्रकृति (अव्यक्त) का कारण होने से वह इससे भी अति परे है। ब्रह्मा से लेकर चींटी और घास के तिनके पर्यन्त जब समस्त सृष्टि का संहार होता है तब भी वह नष्ट नहीं होता। (निरूपण -XV.17)
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।।२१ ।।
शब्दार्थ : अव्यक्तः- अव्यक्त, अक्षरः- अनश्वर, इति-इस प्रकार, उक्तः-कहा गया, तम् - उसे, आहुः-कहते हैं, परमाम् -परम, गतिम् - लक्ष्य, यम् जो, प्राप्य-प्राप्त कर के, न-नहीं, निवर्तन्ते-लौटते, तत्-वह, धाम- स्थान, परमम् सर्वोच्च, मम-मेरा ।
अनुवाद : जो अव्यक्त और "अक्षर" नाम से अभिहित है वही सर्वोच्च लक्ष्य कहा गया है। जो इसे प्राप्त कर लेते हैं वे पुनः इस संसार में नहीं लौटते । वही मेरा परम धाम है।
व्याख्या : परब्रह्म को अव्यक्त कहते हैं क्योंकि वह इन्द्रियों द्वारा दृष्टिगोचर (अनुभवगम्य) नहीं है। इसे अविनाशी भी कहा जाता है। यह सर्वव्यापक, सर्वपारगम्य और अन्तर्व्याप्त है। परब्रह्म सर्वोच्च लक्ष्य है। इससे उच्चतर अन्य किंचिदपि (कुछ भी) नहीं। यह समस्त प्रकार के सीमित अनुबन्धों अथवा अतात्त्विक गुणों से मुक्त शुद्ध अद्वैत-अवस्था है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी इससे गौण है। केवल आत्म-साक्षात्कार द्वारा ही मनुष्य संसार से मुक्त हो सकता है। (निरूपण –XII.3.XV.6.)
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ।।२२ ।।
शब्दार्थ : पुरुषः पुरुष, सः- वह, परः- परम, पार्थ-हे पार्थ, भक्त्या-भक्ति भाव से, लभ्यः- प्राप्त करने योग्य, तु-निःसन्देह, अनन्यया-अनन्य, यस्य-जिसके, अन्तः स्थानि-भीतर निवसित, भूतानि-प्राणी, येन-जिसके द्वारा, सर्वम् सब, इदम् यह, ततम् व्याप्त है।
अनुवाद : हे अर्जुन, जिस परम पुरुष परमात्मा के द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है और समस्त प्राणी जिस परम पुरुष में अन्तर्व्याप्त हैं वह केवल अनन्य भक्ति भाव से ही प्राप्य है।
व्याख्या : समस्त प्राणी (कार्य जगत्) पुरुष में वास करते हैं जो कारण स्वरूप हैं क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने कारण में ही विद्यमान रहता है। जिस प्रकार से एक मिट्टी का पात्र (जो कार्य रूप में है), अपने कारण मिट्टी में रहता है उसी प्रकार सब प्राणी और समस्त लोक अपने कारण रूप पुरुष में अधिष्ठित हैं।
शंकराचार्य के अनुसार अनन्य भक्ति, ज्ञान अथवा आत्मा के ज्ञान के लिए अभिहित है।
'पुरुष' इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु इससे व्याप्त हो जाती है। पुरुष शब्द पुर् धातु से बना है जिसका अर्थ है भरना। पुरि शेते इति पुरुषः अर्थात् जो सब शरीरों में शयन करता है।
इससे बढ़कर अन्य कुछ नहीं, अतः परम पुरुष कहा जाता है। (निरूपण - IX.4; XI.38; XV.6,7)
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ।। २३ ।।
शब्दार्थ : यत्र-जहाँ, काले-समय में, तु-निश्चित रूप से, अनावृत्तिम् -पुनः न लौटना, आवृत्तिम् लौटना, च-और, एव -भी, योगिनः- योगी, प्रयाताः-त्यागते हुए, यान्ति जाते हैं, तम् उस, कालम् समय को, वक्ष्यामि कहूँगा, भरतर्षभ-हे भरत श्रेष्ठ ।
अनुवाद : हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं काल की उस गति के विषय में कहूँगा जिसमें देह त्यागने पर योगी जन पुनः इस भौतिक जगत् में नहीं लौटते और उस गति का भी वर्णन करूँगा जिसमें शरीर त्यागने पर उन्हें पुनः लौटना पड़ता है।
व्याख्या : जिस समय हे भरतश्रेष्ठ, शरीर त्यागने पर योगी का पुनर्जन्म नहीं होता और जिस काल में त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, इन दोनों कालों का उपदेश करूँगा।
आवृत्ति का अर्थ है पुनः जन्म लेना ।
अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।।२४ ।।
शब्दार्थ : अग्निः-अग्नि, ज्योतिः-प्रकाश, अहः-दिवस, शुक्लः- शुक्ल पक्ष, षण्मासाः-छः मास, उत्तरायणम्-उतरायण (सूर्य का उत्तरी पथ), तत्र- वहाँ, प्रयाताः- ले जाये गये, गच्छन्ति-जाते हैं, ब्रह्म-ब्रह्म को, ब्रह्मविदः- ब्रह्मज्ञानी, जनाः लोग।
अनुवाद : अग्नि, प्रकाश, दिवस, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण में जब सूर्य की गति हो-इस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं।
व्याख्या : यह उत्तर मार्ग अथवा देवयान है जो प्रकाश का पथ है। इस पथ से जाने वाले योगी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह पथ मोक्ष प्रदायक है। यह योगी को ब्रह्म लोक ले जाता है। उत्तरायण के छः मास जनवरी के मध्य से ले कर जुलाई के मध्य काल तक हैं। मृत्यु के लिए यह श्रेष्ठ समय कहा जाता है। छान्दोग्योपनिषद्, कौषितकी उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र अध्याय IV.3.4. ii. 18 और 21 में इसका विस्तृत वर्णन है।
"सुविज्ञात होने के कारण प्रकाश पथ से, प्रयाण करने वाला आत्मा क्रमशः आगे बढ़ता है।"
"देवयान पर पहुँचने के उपरान्त वह अग्नि के अधिष्ठातृ देव के लोक को, वायु देव के लोक को, वरुण देव के लोक को, इन्द्र (देवों का राजा) के
लोक को, प्रजापति (सृष्टिकर्ता) के लोक को होते हुए ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है ।''
"वे ज्योतिर्पथ से जाते हैं, ज्योति से दिवस, दिवस से शुक्ल पक्ष, चन्द्र के शुक्ल पक्ष से छः मास जब सूर्य उत्तरायण में होता है, उन मासों से संवत्सर और संवत्सर से सूर्य को प्राप्त होते हैं।"
"मनुष्य इस लोक को त्यागने के पश्चात् वायु लोक में आता है। चक्र में छिद्र की भाँति वायु देव उसके लिए स्थान बनाता है और उसी छिद्र से वह ऊर्ध्वारोहण करता हुआ सूर्य के पास आता है।"
“चन्द्रमा से प्रकाश (विद्युत), वहाँ से कोई अमानव उसे ब्रह्म की ओर अग्रसर करता है।"
काल का वर्णन यहाँ मार्ग अथवा मार्ग की अवस्था का संकेत करता है। अग्नि और प्रकाश (ज्योति) काल के अभिमानी देवता हैं। दिन का अभिमानी देवता दिवसकाल है। शुक्लपक्ष का अपना अधिष्ठाता देव है। उत्तरायण के छः मास का अधिष्ठातृ देवता वही है जो उत्तर मार्ग का अधिष्ठाता है। यह प्रकाश पथ है जो मोक्ष की ओर ले जाता है।
आत्मज्ञान प्राप्त मुक्तात्माओं के श्वास प्रयाण नहीं करते, ब्रह्मलीन होते हैं। जीवन्मुक्त, जिसने कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लिया है, सद्यः मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त कर लिया है उन्हें कहीं जाना नहीं और कहीं से लौटना नहीं। वे सर्वव्यापक परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं।
प्रत्येक चरण (सोपान) एक नवीन चेतना के धरातल पर पड़े, शुद्धता के स्तर में बढ़े और प्रकाशमय हो । जितनी अधिक शुद्धता होगी उतनी ही अधिक दिव्य ज्योति प्राप्त होगी। इस सम्पूर्ण पथ पर ज्योतिर्मय देदीप्यमान् विषय हैं। इस पथ से जाने पर ज्ञान का प्रकाश ही दृष्टिगत होता है अर्थात् प्रकाश की ही अनुभूति होती है। इसीलिए यह प्रकाश-पथ कहा जाता है।
घायल होने पर भी भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े रहे और उत्तरायण के आने पर शरीर त्याग कर ब्रह्म लोक पहुँचे ।
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ।। २५ ।।
शब्दार्थ : धूमः- धूम (धुआँ), रात्रिः रात्रि, तथा तथा, कृष्णः-कृष्णा (कृष्ण पक्ष), षण्मासाः-छः मास, दक्षिणायनम् -सूर्य का दक्षिण पथ, तन्त्र-वहाँ, चान्द्रमसम् चन्द्र, ज्योतिः प्रकाश, योगी-योगी, प्राप्य-प्राप्त करके, निवर्तते-लौटता है।
अनुवाद : जिस मार्ग में धूम, रात्रिकाल, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन के छः मास (जब सूर्य दक्षिण पथ पर हो) हैं-इन मार्गों से होता हुआ चन्द्र ज्योति को प्राप्त कर के योगी वापिस लौटता है।
व्याख्या : यह पितृयान, अन्धकारमय पथ अथवा पितरों के लोक को ले जाने वाला मार्ग है और जहाँ से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। फल की कामना से देवताओं के लिए यज्ञादि एवम् अन्य दान कर्म करने वाले इसी पथ से चन्द्रलोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर इस भूलोक में पुनः अवतरित होते हैं। धूम, रात्रिकाल, कृष्णपक्ष, और दक्षिणायन के छः मास, सब देव हैं जिन्हें अधिष्ठातृ देवता कहा जाता है। वे अज्ञान, आसक्ति और मोह के प्रतीक हैं। पूर्ण पथ में धूम और कृष्ण वर्ण के पदार्थ हैं। इस पथ से जाने पर प्रकाश नहीं दिखता। अज्ञानवश इस पथ से जाते हैं इसीलिए इसे धूममार्ग अथवा अन्धकारमय पथ कहा जाता है।
शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ।।२६ ।।
शब्दार्थ : शुक्लकृष्णे-शुक्ल (प्रकाश) और कृष्ण (अन्धकार), गती-(दो) पथ, हि-निस्सन्देह, एते-ये, जगतः - जगत् के, शाश्वते - शाश्वत, मते-माने जाते हैं, एकया-एक से, याति - (वह) जाता है, अनावृत्तिम् - वापस न आने के लिए, अन्यया-दूसरे के द्वारा, आवर्तते - (वह) लौटता है, पुनः पुनः ।
अनुवाद : संसार के शुक्ल और कृष्ण पथ निश्चित रूप से शाश्वत है। शुक्ल पथ से जाकर लौटना नहीं पड़ता जबकि कृष्ण पथ से जा कर मनुष्य को पुनर्जन्म लेना पड़ता है।
व्याख्या : शुक्ल पथ देव मार्ग है जिसका अनुसरण भक्तगण करते हैं और कृष्ण पथ पितृ मार्ग है जिस पर फल की इच्छा से यज्ञ दानादि क्रियायें करने वाले मनुष्य अनुगमन करते हैं। ये दोनों मार्ग सम्पूर्ण विश्व के लिए नहीं हैं। शुक्ल पथ (देवयान) भक्तों के लिए और कृष्ण पथ (पितृयान) अनुष्ठानों में आस्था रखने वालों के लिए है। ये दोनों पथ इतने ही शाश्वत हैं जितनी यह सृष्टि । "जगतः" का अभिप्राय यज्ञादि क्रियाओं में आस्था रखने वाले भक्तों से है। पितृलोक अथवा चन्द्रलोक स्वर्गलोक है।
नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।।२७ ।।
शब्दार्थ : न नहीं, एते-ये, सृती-दो पथ, पार्थ-हे पार्थ, जानन्-जानते हुए, योगी-योगी, मुह्यति-मोहित होता है, कश्चन-कोई, तस्मात् -इसलिए, सर्वेषु सब, कालेषु-कालों में, योगयुक्तः - योग परायण, भव-बनो, अर्जुन-हे अर्जुन ।
अनुवाद : हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों का ज्ञान होने पर योगी मोहित नहीं होता, इसलिए, हे पार्थ, तुम सब कालों में योग युक्त रहो अर्थात् योगी बनो ।
व्याख्या : दोनों मार्गों की प्रकृति और उनके परिणाम जानते हुए योगी विवेकशून्य नहीं होता। यह ज्ञान हो जाने पर कि देवयान अथवा प्रकाश-पथ मोक्ष (क्रम मुक्ति) प्रदायक है और पितृयान अथवा अन्धकार पथ आवागमन (जन्म-मृत्यु) के चक्र में घुमाने वाला है, योगी मोहित नहीं होता। इन दोनों मार्गों का ज्ञान प्रतिक्षण योगी के लिए संकेत-दीप (पथ-प्रदर्शक) का कार्य करता है। वह प्रकाश-पथ पर अडिग बने रहने की आकाङ्क्षा रखता है।
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ।।२८ ।।
शब्दार्थ : वेदेषु वेदों में, यज्ञेषु यज्ञों में, तपःसु-तपों में, च-और, एव-भी, दानेषु उपहारों में, यत्-जो भी, पुण्यफलम् -पुण्यफल, प्रदिष्टम् -घोषित किया गया है, अत्येति-परे चला जाता है, तत्-उस, सर्वम् -सब, इदम् -यह, विदित्वा-जान कर, योगी-योगी, परम् -परम, स्थानम् धाम को, उपैति -प्राप्त करता है, च और, आद्यम् सनातन ।
अनुवाद : इस तत्त्व को जान कर योगी वेदाध्ययन, यज्ञादि अनुष्ठान, तप और दान से प्राप्त होने वाले शास्त्र-विहित पुण्य फल से परे (ऊपर) चला जाता है और परम सनातन पद को प्राप्त करता है।
व्याख्या : इस श्लोक में योग की महिमा वर्णित है। वेदों के अध्ययन से, समुचित रूप से किये गये अनुष्ठान के अभ्यास से, तप करने से प्राप्त होने वाले जो-जो भी शास्त्रों के अनुसार (शास्त्र-निर्दिष्ट) पुण्य फल हैं-ब्रह्मनिष्ठ योगी जो भगवान् कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिये गये सात प्रश्नों के उत्तर में उपदेश हैं, उनका अनुसरण करता है वह इन समस्त (पुण्य फल आदि) से अतीत है। वह पर ब्रह्म के सनातन परम धाम को प्राप्त करता है जिसका अस्तित्व सृष्टि के आदि काल में भी था।
इदं विदित्वा-यह जान कर । इस अध्याय के प्रारम्भ में अर्जुन द्वारा पूछे गये सात प्रश्नों के उत्तर रूप दिये गये भगवान् कृष्ण के उपदेश को भली प्रकार जान कर ।
(इस अध्याय को अभ्यास-योग भी कहा जाता है।)
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ।।८ ।।
।। इति अक्षरब्रह्मयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ नवमोऽध्यायः
राजविद्याराजगुह्ययोगः
श्री भगवानुवाच
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ।।१ ।।
शब्दार्थ : इदम् - यह, तु-निश्चित रूप से, ते-तुम्हारे लिए, गुह्यतमम् -परम गोपनीय, प्रवक्ष्यामि कहूँगा, अनसूयवे-दोष रहित, ज्ञानम् - ज्ञान, विज्ञानसहितम् - विशेष ज्ञान सहित (अनुभव सहित), यत्-जो, ज्ञात्वा-जान कर, मोक्ष्यसे-मुक्त हो जाओगे, अशुभात् -अशुभ से ।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : (हे अर्जुन), तुम दोष रहित हो अतः अब मैं तुम्हारे लिए आत्म ज्ञान के अनुभव सहित परम-गोपनीय (रहस्यमय) ज्ञान का उपदेश करूँगा। इस ज्ञान को प्राप्त कर के तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे।
व्याख्या : इदम् यह, अर्थात् आत्म ज्ञान
ज्ञान-उपनिषदों के अध्ययन द्वारा प्राप्त ब्रह्म का सैद्धान्तिक ज्ञान अथवा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ।
विज्ञान-आत्म साक्षात्कार अथवा अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान । संसार के बन्धन से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति और अशुभ अर्थात् संसार के दुःखों से छुटकारा पाने का केवल यही सहज उपाय है।
आत्म ज्ञान परम गोपनीय है। शब्दों में इसका वर्णन करना अत्यन्त कठिन है। अपरोक्षानुभूति अथवा आध्यात्मिक अन्तर्प्रज्ञा से ही यह ज्ञान सम्भव है। आत्मा, ब्रह्म, आत्म ज्योति, सनातन परम पुरुष मनुष्य के हृदय प्रकोष्ठ में सदैव विराजित रहता है। युगों युगों से आध्यात्मिक पथ पर अनुगमन करने वाले मनुष्य अल्पता में ही रहे हैं जिन्होंने आत्मा के अमोघ मोती रूप आध्यात्मिक कोष के इस रहस्य को जाना। मोक्ष प्राप्ति हेतु आत्म ज्ञान ही सरल साधन है। कर्मयोग हृदय को परिमार्जित कर के आत्म ज्ञान की ओर अग्रसर करता है।
भगवान् कृष्ण कहते हैं-"हे अर्जुन, क्योंकि तुम ईर्ष्या-द्वेष से मुक्त हो, मैं तुम्हारे लिए अनुभवगत दुर्बोध रहस्यात्मक ज्ञान का उपदेश करूँगा"। इससे यह स्पष्ट है कि साधक के लिए अनसूय होना एक महान् गुण है। प्रचंड हृदय-दहन (जलन) उत्पन्न करने वाली और मन को अन्य मनस्क (उद्विग्न) करने वाली ईर्ष्या से मुक्त मानस में ही ज्ञान का सूर्य उदित हो सकता है। मत्सर्य (दुर्भाव पूर्ण ईर्ष्या), ईर्ष्या (दूसरों के सुख-सम्पत्ति से ईर्ष्या), असूया (दूसरों के गुणों से ईर्ष्या) ये सब ईर्ष्या के विभिन्न प्रकार हैं। यदि तुम एक गुणी व्यक्ति पर दुर्गुणों का आरोपण करो जो वास्तव में इन सब से पृथक् है और तुम उसके लिए कुछ बुरा कहते हो तो यह असूया है। छिद्रान्वेषण की दृष्टि से किसी भले और गुणी व्यक्ति को देखना, जो वस्तुतः इन बुराइयों से मुक्त है, असूया है। ईर्ष्या (असूया) तो मात्र मन की लघुता को दर्शाती है। यह अज्ञान का परिवर्तित रूप है। आत्म परिप्रश्न द्वारा इसे दूर किया जा सकता है अथवा हृदय की विशालता, महानता, उदार-सार्वभौमिकता और श्रेष्ठता आदि विपरीत गुणों के विकास से असूया मुक्त हो सकते हैं।
अनसूयवे-इसका अभिप्राय है कि अर्जुन एक गुणी शिष्य के समस्त गुणों-ऋजुता (सरलता), आत्म संयम, इन्द्रिय संयम, सौम्यता, विवेक, अनासक्ति आदि से युक्त था। यह उपलक्षणा है (जहाँ सत्य के एक अंश का संकेत है और असूया उपलक्षक है जो उपलक्षण का संकेत है)।
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्।।२।।
शब्दार्थ: राजविद्या-विद्याओं में राजा (अतिशय देदीप्यमान और प्रकाशयुक्त होने के कारण ब्रह्म विद्या सब विद्याओं का राजा है) राजगुह्यम्-सब रहस्यों का राजा, पवित्रम् -पवित्र, इदम् -यह, उत्तमम् -सर्वश्रेष्ठ, प्रत्यक्षावगमम् - अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) अन्तदृष्टि द्वारा जिसका ज्ञान हो सके, धर्म्यम् धर्मयुक्त, सुसुखम् - अत्यन्त सहज, कर्तुम् -करने में, अव्ययम्-अविनाशी ।
अनुवाद : यह राजविद्या है, राजर्षियों का रहस्य है, अत्यन्त पावनी है, प्रत्यक्ष रूप से बोधगम्य है, धर्म के अनुरूप है, करने में सहज है और अविनाशी है।
व्याख्या : तत्काल ज्ञान प्राप्ति हेतु आध्यात्मिक साधक को प्रेरित करने और उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए भगवान् कृष्ण इस श्लोक में ब्रह्मज्ञान की बहुत प्रशंसा करते हैं।
इस 'राजविद्या' में न तो अन्धविश्वास है और न ही विश्वास का व्यापार (अर्थात् पूर्ण निष्ठा से सफलता निश्चित है) । सत्य, सार्वभौम रहस्य (आत्मन्, पाम सत्य) देहातीत, भावातीत ज्ञान से तत्काल जाना जा सकता है। समस्त विद्याओं में परमात्मा का विज्ञान (विद्या) सर्वाधिक भव्य है, उत्कृष्ट है। यह विज्ञानों का विज्ञान है। विज्ञानों में सर्वोच्च, रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय और पवित्र करने वाले शोधकों में यह सर्वोत्तम है। ब्रह्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ शोधक है। समस्त कर्मों को यह जड़ से उखाड़ देने वाला है। ब्रह्मज्ञान से, पलक झपकते ही सहस्रों जन्मों के संचित कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। यह अविद्या को कार्य (प्रभाव) सहित नष्ट करता है। प्रायश्चित कर्म से सारे पाप नष्ट नहीं हो सकते। कुछ सीमा तक यह किसी एक पाप के प्रभाव को नष्ट करने में सक्षम है। इसे हटाया भी जाये तो भी इसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से मन में रहता है जो आगामी जन्म में पुनः अमूरित हो कर साधक को वही पाप करने के लिए बाध्य करता है। किन्तु ब्रह्मज्ञान जन्मों-जन्मों से संचित पापों को उनकी स्थूल और सूक्ष्म दोनों अवस्थाओं में मूलकारण अविद्या सहित तत्काल नष्ट करता है। इसीलिए यह परम शोधक कहा गया है। जीव का कारण शरीर मूल-अविद्या कहा गया है। अविद्या अथवा अज्ञान का आवरण जो संसार के दृश्य पदार्थों को ढके हुए है, वह स्थूल अविद्या है।
आत्म ज्ञान, धर्म का विरोध नहीं है। यह तो अनेक जन्मों में निष्काम भाव से किये गये कर्मों का प्रतिफल है। पुनरपि, आत्म ज्ञान सहज ही प्राप्त हो सकता है। विचार उठ सकता है कि इतना सहज यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो प्रभाव क्षीण होने पर यह लुप्त भी हो सकता है। किन्तु ऐसा नहीं है। यह ज्ञान अविनाशी है। यह नित्य है। अपने ही प्रकाश से यह सदा प्रकाशित रहता एक बार इसका स्वाद ले लेने पर मनुष्य अमर हो जाता है। अतः आत्म ज्ञान तो निश्चित रूप से प्राप्त करने योग्य ही है। येन केन प्रकारेण इसे इसी जन्म में प्राम करना अत्यन्त आवश्यक है, कौन जाने, पुनः यह मानव-तन मिले न मिले। प्रत्येक क्षण संघर्ष करो क्योंकि जीवन अनिश्चित है और पुरस्कार (मोक्ष) महान् है।
अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ।।३ ।।
शब्दार्थ : अश्रद्दधानाः श्रद्धारहित, पुरुषा:-पुरुष, धर्मस्य-धर्म (कर्तव्य) का, अस्य-इस, परंतप -शत्रु संहारक (अर्जुन), अप्राप्य-प्राप्त न कर के, माम् -मुझे, निवर्तन्ते-लौटते हैं, मृत्युसंसारवत्र्मनि-मर्त्य लोक के इस पथ में।
अनुवाद : हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म (आत्मज्ञान) में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त किये बिना ही इस मर्त्य लोक में पुनः लौटते हैं।
व्याख्या : अर्जुन प्रश्न करते हैं- "भगवन्, जब यह ज्ञान सब प्रकार से कल्याणप्रद है, सर्वोच्च है, सहज भी है तो लोग इसे प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करते? निश्चयेन, सब को आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए?" भगवान् उत्तर देते हैं-"हे मेरे प्रिय शिष्य, लोगों को इस ज्ञान में विश्वास नहीं है अतः पुनः-पुनः वे इस मर्त्य लोक में लौटते हैं। निज कल्पना के साधनों से यदि वे प्रयास करते भी हैं तो भी वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र-विहित सम्यक् साधनों और नियमों से वे वंचित हैं।"
धर्म का अर्थ है नियम, धर्म, आत्म ज्ञान ।
यह विश्वास, मात्र बौद्धिक विश्वास नहीं है जो किसी मत अथवा सिद्धान्त का मताग्रही हो। किसी दूसरे की अभ्युक्ति का भी मात्र विश्वास नहीं है। यह अविचल, अटल, आन्तरिक धारणा है कि आत्म ज्ञान से ही परम शान्ति, अमृतत्व और शाश्वत आनन्द प्राप्त हो सकता है। शंकराचार्य का यही प्रबल, अटूट विश्वास था जिसके कारण परम शोधक, भावातीत, धर्मानुरूप, सहज और अविनाशी ज्ञान प्राप्ति हेत् उन्होंने अपनी माताश्री का त्याग कर के श्री भविन्दपाद गुरु की अहेतुकी शरण प्राप्त की। महात्मा बुद्ध के इसी दृढ़-निश्चय मे गोले आलेय धारणा धारण करने को प्रेरित किया। उनके ही अपने शब्दों कुटे "जब तक मुझे प्रकाश (बोध) नहीं होता, मैं अपने आसन से एक इंच भी नहीं हिलूँगा।" आग्नेय संकल्प के साथ विश्वास साथ-साथ ही चलता है।
भगवान् कृष्ण ने प्रथम दो श्लोकों में आत्म ज्ञान की प्रशंसा सकारात्मक विधि (विधि मुखस्तुति) से की है। तीसरे श्लोक में उन्होंने इसका गुणगान निषेधात्मक विधि (निषेध मुखस्तुति) से किया है। आत्म ज्ञान-प्राप्ति के लाभों का वर्णन प्रथम और द्वितीय श्लोक में है। यह विधि मुखस्तुति है। आत्म ज्ञान प्राप्त न करने से अनर्थकारी (विपत्तिजनक) परिणामों का वर्णन तृतीय श्लोक में है। यह है-निषेध मुखस्तुति ।
लालची, कामुक और पापी मनुष्य जो देह दर्शन के अनुयायी हैं, राक्षसों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, देह को ही आत्मा मान कर इसकी पूजा करते हैं और जिन्हें आत्म ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, वे मुझे प्राप्त नहीं होते। उनके पास तो मेरी ओर आने के लिए अल्प मात्र भक्ति भी नहीं है। वे तो मर्त्य लोक पथ पर आरूढ़ होते हैं जो नरक और कीट, पशु आदि योनियों में ले जाने वाला है।
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।।४ ।।
शब्दार्थ : मया-मेरे द्वारा, ततम् व्याप्त, इदम् यह, सर्वम् सब, जगत् -संसार, अव्यक्तमूर्तिना-अव्यक्त रूप से, मत्स्थानि-मुझ में वास करते हैं, सर्वभूतानि समस्त प्राणी, न-नहीं, च-और, अहम् -मैं, तेषु उनमें, अवस्थितः - स्थित हूँ।
अनुवाद : समस्त जगत् में अव्यक्त रूप से मैं ही व्याप्त हूँ। सब जीव मुझ में स्थित हैं किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ।
व्याख्या: अव्यक्त मूर्ति-पर ब्रह्म अथवा दृष्टि द्वारा अगोचर परम सत्ता है जिसे आध्यात्मिक भावातीत ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। ब्रह्मा, सुटि कर्ता से लेकर तृण और चींटी पर्यन्त सारे जीव पर ब्रह्म में स्थित है। उनका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। वे उस परम सत्ता के द्वारा जीवित हैं जो सब में अन्तर्निहित है। इसका कोई आधार नहीं है क्योंकि ब्रह्म ही सब जीवों का आत्म हैं कि वह उनमें वास करता है किन्तु ऐसे हो भी कैसे सकता है? अनन्त सत्ता सीमित में कैसे समा सकती है? ब्रा का किसी भौतिक पदार्थ से कोई सम्पर्क नहीं है। कुर्सी या मेज का धरती से सम्पर्क हो सकता है या मनुष्य और किताब का, किन्तु ब्रह्म का ऐसा सम्पर्क नहीं है। इसीलिए उन प्राणियों में वह वास नहीं करता। जिसका किसी पदार्थ अथवा प्राणी से सम्बन्ध ही नहीं है उसे कहीं भी, जैसे किसी पात्र, बाक्स, कक्ष अथवा आधान में नहीं रखा जा सकता। आत्म तत्त्व इन रूपों में मूलबद्ध नहीं है। जिस प्रकार से समस्त रूप आकाश से प्रकट होते हैं किन्तु आकाश को किसी रूप में आबद्ध नहीं कर सकते उसी प्रकार ब्रह्मन् किसी रूप में आबद्ध नहीं है। वह निराकार है।
सारे प्राणी ब्रह्म में वास करते प्रतीत होते हैं किन्तु यह एक भ्रम है। यह भ्रम दूर हो जाये तो ब्रह्म के अतिरिक्त शेष कुछ भी न रहे। इस भ्रम का कारण अज्ञान जब नष्ट होगा तो इन प्राणियों के अस्तित्व का विचार भी लुप्त हो जाएगा।
श्लोक ४ और ५ में भगवान् ने एक विरोधाभास दिया है। “समस्त प्राणी मुझ में वास करते हैं। किन्तु वास करते हुए भी मुझमें वास नहीं करते और मैं उनमें वास नहीं करता" । एक चिन्तनशील व्यक्ति के लिए यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। जिस प्रकार आकाश में सब कुछ स्थित है पुनरपि स्पर्श से परे है उसी प्रकार पर ब्रह्म में सब पदार्थ हैं पुनरपि उनके स्पर्श से परे हैं अर्थात् ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकते (आकाश की भाँति) । मूल प्रकृति भी जो इस संसार का स्रोत है, ब्रह्म पर आश्रित है किन्तु ब्रह्म का कोई आधार अथवा मूल नहीं है। यह तो अपनी ही आदि और विलक्षण महिमा में आश्रित है। (निरूपण- - VII.12, 24; VIII .22 )
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।।५ ।।
शब्दार्थ: न नहीं, च और, मत्स्थानि मुझ में आश्रित, भूतानि-प्राणी, परम-देखो, मे मेरे, योगम्-योग को, ऐश्वरम् -दिव्य, भूतभृत्-प्राणियों का पोषण करते हुए, न-नहीं, चऔर, भूतस्थः -प्राणियों में स्थित, मम-मेरी, सोना आत्मा, भूतभावनः - भूतों को उत्पन्न करने वाला।
अनुवाद : (वस्तुतः) जीव मुझ में स्थित नहीं है। मेरे दिव्य योग को रेडो कि मेरा आत्मा प्राणियों को उत्पन्न करने और उनका पोषण करने वालो होते हुए भी उनमें स्थित नहीं है।
व्याख्या : ब्रह्म सूक्ष्मतम है, निराकार है अतः इसका किसी पदार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए यह असङ्ग है। पदार्थ और आत्म तत्त्व में कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। साकार (रूप सहित) का निराकार (रूप रहित) से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।
यह हो भी कैसे सकता है?
अनासक्त कभी आसक्त नहीं होता।
(असङ्गो न हि सज्यते) बृहदारण्यक उपनिषद् (III.9.26)
अनासक्त होते हुए भी यह प्राणियों का पोषण करता है। यह कर्त्ता है। सम्पूर्ण सृष्टि का उद्भव इससे है किन्तु स्वयं उसमें वास नहीं करता क्योंकि यह किसी भी विषय से असम्बद्ध है। यह एक महान् रहस्य है। एक स्वप्नद्रष्टा को जैसे स्वप्न के विषय से कोई प्रयोजन नहीं होता, आकाश और वायु को पात्र से कोई प्रयोजन नहीं होता इसी प्रकार ब्रह्म को भौतिक पदार्थों से कोई प्रयोजन नहीं। भौतिक शरीर और आत्मा का सम्बन्ध तो एक भ्रम है। प्रातिभासिक पदार्थों का अधिष्ठान (ब्रह्म) जो ब्रह्म पर आरोपित किया गया है, उसका विषयों के गुण-दोषों से कोई सम्बन्ध नहीं। सर्प रज्जु पर अध्यारोपित है। कल्पित सर्प के लिए रज्जु अधिष्ठान है। यह अध्यास का एक दृष्टान्त है। (निरूपण-VII.25; X.7; XI.8)
यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।।६ ।।
शब्दार्थ : यथा-जैसे, आकाशस्थितः- आकाश में स्थित, नित्यम् सदा, बाहु-वायु, सर्वत्रगः सर्वत्र गति करता है, महान् -महान्, तथा-वैसे ही, सर्वाणि-समस्त, भूतानि-प्राणी, मत्स्थानि-मुझ में स्थित हैं, इति-इस प्रकार, उपधारय जानो ।
अनुवाद : जिस प्रकार सर्वत्र विचरण करने वाला वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है उसी प्रकार सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो।
व्याख्या : प्रथम दो श्लोकों में दी गयी व्याख्या को और अधिक साक करने के लिए भगवान् उपमा दे रहे हैं। जिस प्रकार वायु असङ्ग हो कर आकार मैं आश्रित है उसी प्रकार समस्त प्राणी बिना किसी सङ्ग के ब्रह्म में स्थित हैं। ये पदार्थ उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते।
ब्रह्माण्ड के पदार्थों और ब्रह्म में किस प्रकार का सम्बन्ध है? यह संयोग, समवाय अथवा तादात्म्य सम्बन्ध है? ड्रम (Drum) के साथ डण्डी का सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध है। अनुमान करो कि सम्बन्ध ऐसा ही है। समस्त भागों के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म अनन्त, असीम है और तत्त्व ससीम है। तुम एकादेश सम्बन्ध स्थापित कर सकते हो किन्तु यह सम्भव नहीं है। क्योंकि ऐसा सम्बन्ध उन विषयों में सम्भव है जिनके या तो सदस्य हैं अथवा भाग हैं जैसे वानर और वृक्ष (एक देश अशंता है) । ब्रह्म अंश रहित है।
यदि समवाय सम्बन्ध का ब्रह्म और पदार्थों के मध्य विचार करें तो यह भी असम्भव है। गुण और गुणधारक के मध्य सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध कहलाता है। एक व्यक्तिगत ब्राह्मण और सम्पूर्ण ब्राह्मण जाति का सम्बन्ध भी समवाय सम्बन्ध है। मनुष्य और उसके हाथ, मनुष्य और उसकी टाँग का सम्बन्ध भी समवाय है। ऐसा सम्बन्ध ब्रह्म और जीव अथवा अन्य पदार्थों में नहीं है।
तीसरे प्रकार का सम्बन्ध है-तादात्म्य सम्बन्ध, जो दूध और पानी, अग्नि और लौह खण्ड में दृष्टिगत होता है। दुग्ध का श्वेत वर्ण और मधुरता जल से मिलते-जुलते हैं। अग्नि का प्रकाश, रक्त वर्ण और उष्णता तप्त लौह खण्ड से मिलते हैं। ब्रह्म, पदार्थ और अन्य तत्त्वों में यह सम्बन्ध भी सम्भव नहीं है; क्योंकि ब्रह्म सत्-चित्-आनन्द, परम, अखण्ड और पूर्ण है जब कि तत्व चेतना-शून्य (जड़) है, सीमित है और दुःखद है। ऐसे विपरीत गुण वाले पदायाँ का ब्रह्म के साथ तादात्म्य सम्बन्ध कैसे स्थापित हो सकता है? इसलिए यह कहना उचित ही है कि तत्वों का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध कल्पित है (अध्यारोपित है)। जो पदार्थ आधार पर आरोपित हैं उसकी सत्ता तो केवल नाम की है। वास्तव में उसका अस्तित्व ही नहीं है। नाम-रूप के इस ससार का आधार ब्रह्म है। संसार का अभिप्राय यहाँ प्राणियों और उनके तीन प्रकार के शरीरों (अन्नमय, मनोमय और कारण शरीर) से है। अतः तत्त्व अथवा प्राणी वस्तुतः ब्रह्म में हरभूत नहीं हैं। वे वास्तव में ब्रह्म में वास नहीं करते। ये केवल नाम हैं।
वायु का अभिप्राय सूत्रात्मन् अथवा हिरण्यगर्भ से भी है। भूत व्यष्टि बेसना है। जिस प्रकार से किसी पात्र के भीतर का आकाश उसके निर्माण और विनाश के पूर्व और पश्चात् और उस पात्र के सत्ता कालों में एक ही है, उसी प्रकार जीवात्मा की प्रकृति तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य में ब्रह्म से पृथक् नहीं है।
जिस प्रकार से समस्त द्रव्य अपने कार्य रूप के अस्तित्व, अस्तित्व से पूर्व और पश्चात् भी अपने उपादान कारण से अभिन्न रहते हैं उसी प्रकार व्यष्टि आत्माएँ अपने विभिन्न अनुबन्धों मन, बुद्धि आदि उद्भव से पूर्व अस्तित्व काल में और विनाश के पश्चात् भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं।
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ।।७ ।।
शब्दार्थ : सर्वभूतानि समस्त प्राणी, कौन्तेय- हे कौन्तेय, प्रकृतिम् -प्रकृति को, यान्ति-जाते हैं, मामिकाम् -मेरी, कल्पक्षये-कल्प के अन्त में, पुन-पुनः, तानि-उन्हें, कल्पादौ-कल्प के आदि में, विसृजामि-भेजता हूँ, बहम्-मैं।
अनुवाद : हे अर्जुन, समस्त प्राणी कल्प के अन्त में मेरी प्रकृति को प्रशाम होते हैं और (आगामी) कल्प में मैं उन्हें पुनः भेजता हूँ।
व्याख्या : प्रकृति-सत्व, रजस् और तमस्, इन तीन गुणों से युक्त मिन प्रकृति। जिस प्रकार घास धरती पर उत्पन्न हो कर उसी में सूख जाती है, अर्मियां (छोटी लहरें) और लहरें सागर से उठ कर उसी में लीन हो जाती हैं, स्वान मन से अस्तित्व में आ कर स्वप्नद्रष्टश के जागृत होने पर मन में ही लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सब प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हो कर प्रलय काल में प्रकृत ही विलीन हो जाते हैं।
प्रलय विघटन (विलोप) की अवधि है। महा-उत्पति रचना-काल है। (निरूपण –VIII.18,19)
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ।।८ ।।
शब्दार्थ : प्रकृतिम् - प्रकृति को, स्वाम्-अपनी, अवष्टष्य -अनुप्रमाणित कर के, विसृजामि-सृजन करता हूँ, पुनः पुनः - पुनः पुनः, कर भूतग्रामम्-भूत समुदाय को, इमम् -इस, कृत्स्नम् -समस्त, अवशम् - परतन्त्र, प्रकृतेः- प्रकृति के, वशात् -वश से।
अनुवाद : अपनी प्रकृति को अनुप्राणित कर के मैं पुनः पुनः समस्त भूत समुदाय को (संसार में) भेजता हूँ जो प्रकृति के आधीन हैं जो असहाय हैं।
व्याख्या : भगवान् प्रकृति को अङ्गीकार करते हैं, समाश्रित करते हैं। आलिंगन करते हैं। महाकल्प अथवा महाप्रलय के उपरान्त सुषुप्त प्रकृति को दे पुनः शक्ति और पुष्टि प्रदान कर के उर्वरक बनाते हैं तथा भूत समुदाय का पुनः सृजन करते हैं। प्रत्येक स्तर और तल पर उद्भव के पश्चात् वे दृष्टिपात करते हैं। 'प्रकृति' शब्द पाँच प्रकार के क्लेशों का संकेत करता है-अज्ञान, अस्मिता (अहंभाव), राग, द्वेष और अभिनिवेश अर्थात् भौतिक जीवन में संलमता । (निरूपण-IV.6)
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ।।९ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, च और, माम् -मुझको, तानि-ये, कर्माणि -कर्म, निबध्नन्ति-बाँधते हैं, धनन्जय -हे अर्जुन,
आसीनम् - बैठे हुए, असक्तम् - अनासक्त, तेषु -उनमें, कर्मसु -कमों में।
अनुवाद : हे अर्जुन, उन कर्मों के प्रति अनासक्त और उदासीन की भाँति बैठे हुए मुझको वे कर्म नहीं बाँधते ।
व्याख्या: तानि कर्माणि-ब्रह्माण्ड की सृष्टि और प्रलय । ब्रह्माण्ड की प्रलय का केवल मैं ही एक कारण है। प्रकृति के उद्भव और विकास का एकमात्र कारण भी मैं है, पुनरपि सब के प्रति विरक्त रहने के कारण मैं कुछ भी नहीं करता। किसी क्रिया का कारण भी मैं नहीं बनता।
मैं समरस, अनासक्त और असम्बद्ध रहता हूँ। उन कर्मों के प्रतिफल की मुझे आसक्ति नहीं है। "मैं कर्ता हूँ, यह अहंभाव भी मुझ में नहीं है। मैं जानता कि आत्मा कर्मरहित है इसलिए सृष्टि की रचना और विघटन मुझे बन्धन में नहीं डालते।
ईश्वर की ही भाँति अन्य मनुष्यों में भी कर्तृभाव का अभाव और कर्मफल में अनासक्ति (धर्म और अधर्म तथा शुभाशुभ में) मोक्ष का कारण है। अज्ञानी मनुष्य अहंभाव से कर्म कर के और फल की इच्छा कर के रेशम-कीट के कृमिकोष में बंधने के समान बन्धन में आ जाता है।
क्रिकेट अथवा फुटबाल मैच में जैसे मध्यस्था (referee) अथवा आम्मायर किसी भी पक्ष की जय-पराजय से प्रभावित नहीं होता वैसे ही भगवान् संसार की सृष्टि और प्रलय से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे इन सबसे उदासीन (विरक्त) रहते हैं और सदा एकरस (अपरिवर्तनशील) मौन द्रष्टश हैं। (निरुपण-IV.14)
मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।।१० ।।
शब्दार्थ : मया-मेरे द्वारा, अध्यक्षेण-अधिष्ठाता के द्वारा, प्रकृतिः- प्रकृति, सूयते-उत्पन्न करती है, सचराचरम्-चर और अचर को (जड़ और चेतनको) हेतुना-कारण से, अनेन-इस, कौन्तेय-हे कौन्तेय, जगत् संसार, विपरिवर्तते-घूमता है।
अनुवाद : हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा चराचर जगत् की संरचना होती है और संसार चक्र परिभ्रमण करता है।
व्याख्या : भगवान् तो केवल द्रष्टा हैं। प्रकृति सब कुछ करती है। उनके सान्निध्य अथवा विद्यमानता के कारण प्रकृति चराचर जगत् को उत्पन्न करती है। सृष्टि का मूल कारण प्रकृति है। जड़, चेतन और समस्त विश्व का मूल कारण प्रकृति है। ।
यद्यपि समस्त कर्म सूर्य के प्रकाश में किये जाते हैं पुनरपि सूर्य कर्मों का कर्ता नहीं बन सकता। इसी प्रकार भगवान् के दिव्य प्रकाश में प्रकृति के सब कार्य होते है पुनरपि भगवान् कर्ता नहीं बन सकते। ब्रह्म संसार के निमित कारणके रूप में अविद्या को प्रकाशित करते हैं अतः यही संसार का कारण मानी जाती है। चुम्बक के सम्पर्क में आये लोहे के टुकड़े घूमने लगते हैं पर चुम्बक उससे प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार भगवान् प्रकृति को सृष्टि की रचना हेतु प्रेरित करते हैं किन्तु स्वयं इससे उदासीन रहते हैं।
व्यक्त और अव्यक्त चराचर वस्तुओं से युक्त इस जगत् में भगवान एक स्वामी और साक्षी के रूप में अधिष्ठाता हैं।
सृष्टि का प्रयोजन क्या है? जब भगवान् को किसी प्रकार के आमोद-प्रमोद से कोई प्रयोजन ही नहीं तो उन्होंने सृष्टि की रचना क्यों की? या अतिप्रश्न (Transcendental) है। अतः यह प्रश्न पूछना अथवा इसका उल देना, दोनों ही असङ्गत हैं। आप यह नहीं कह सकते कि भगवान् ने जाने मनोरंजन के लिए यह संसार रचा क्योंकि वे तो इन सब से परे हैं और मात्र तु हैं। (निरूपण-X.8)
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ।।११ ।।
शब्दार्थ : अवजानन्ति-अवज्ञा करते हैं, माम् -मुझे, मूढ़ा-मूर्ख, मानुषीम् -मनुष्य रूप, तनुम् - शरीर, आश्रितम् - धारण किए हुए, परम्-उच्चतर, भावम् -भाव को, अजानन्तः -न जानते हुए, मम-मेरी, भूतमहेश्वरम् -सब जीवों के महेश्वर ।
अनुवाद : समस्त प्राणियों के स्वामी के रूप में मेरे उच्चतर अस्तित्व से अनभिज्ञ और मेरे परम भाव को न जानते हुए मूर्ख लोग मनुष्य रूप में मुझ महेश्वर की अवज्ञा करते हैं।
"व्याख्या : जिस प्रकार पीलिया के रोगी को सर्वस्व पीला ही दिखाई देता है इसी प्रकार केवल मूर्ख ही मेरी पावन प्रकृति में दोष देखते हैं। ज्वरग्रस्त होगी को यदि मधुर दुग्ध भी दें तो उसे नीम जैसा कड़वा प्रतीत होगा। भौतिक नेत्रों से मेरा दर्शन करने के इच्छुक मुझे नहीं जान सकते। मरीचिका (मृग तृष्णा) को यदि कोई गंगा समझे तो क्या वह जल प्राप्त कर लेगा?
विवेक शून्य और ज्ञान शून्य मूर्ख जन, मनुष्य रूप धारण किये मेरी उपेक्षा करते हैं। मैंने अपने भक्तों के उद्धार के लिए यह शरीर धारण किया है। मेरे उच्च भाव का इन्हें ज्ञान नहीं। वे नहीं जानते हैं कि मैं महेश्वर हूँ, परम आत्मा हूँ, ज्योतिर्मय, सर्वज्ञ, पवित्र, सदा मुक्त, अमर, प्रज्ञावान् और सब का आत्मा हूँ। ये मूर्ख मुझे साधारण मानव समझ कर मेरा तिरस्कार करते हैं। बुद्धिमान् मेरी आध्यात्मिक प्रकृति और अभिव्यक्त प्रकृति को जानते हैं।
ब्रह्माण्ड में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ, अन्तर्व्याप्त हूँ। इस संसार का मैं आलम्बन हूँ। शरीर, मन, प्राण, इन्द्रियों का आधार मैं हूँ पुनरपि कुछ शोचनीय मूढ़ हैं जो मेरे अस्तित्व को नकारते हैं। मेरे अस्तित्व से कोई स्थान खाली नहीं किन्तु ये लोग मुझे देख नहीं पाते। इनका भाग्य ही शोचनीय है। (निरूपण-IV.6; VII.24)
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ।।१२ ।।
शब्दार्थ : मोघाशाः व्यर्थ आशा वाले, मोघकर्माणः व्यर्थ कर्म वाले, मोघज्ञानाः- व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसः-अज्ञानी, राक्षसीम् -राक्षसी, आसुरीम् - आसुरी (अदिव्य), च-और, एव-ही, प्रकृतिम् - प्रकृति को, मोहिनीम् - भ्रमित करने वाली, श्रिताः युक्त हैं।
अनुवाद : व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले ये अज्ञानी लोग राक्षसी, अदिव्य, भ्रामक प्रकृति से युक्त हैं।
व्याख्या : वे व्यर्थ की आशाओं का आश्रय लेते हैं क्योंकि नश्वर रूपों मैं तो कोई आशा हो ही नहीं सकती। आशा व्यर्थ इस भाव में है कि वे शाश्वत को छोड़ कर क्षणिक पदार्थों के पीछे भागते हैं। यह एक व्यर्थ कर्म है क्योंकि यह भगवान् को समर्पित करके नहीं किया गया। केवल अग्निहोत्र तथा अन्य क जो वे करते हैं, सब निष्फल है क्योंकि वे अन्तरात्मा रूप भगवान् का तिरस्का करते हैं। वे अज्ञानी है क्यों कि उनमें विवेक नहीं है। शाश्वत आत्म तत्त्व का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वे तो अपने शरीरों की पूजा करते हैं। शरीर से पसेके आत्मा को नहीं देखते । अपनी ही आत्मा की वे उपेक्षा करते हैं। वे अत्याचा और पाशविक कर्म करते हैं। वे दूसरों का धन लूटते हैं और हिंसा करते है इसीलिए वे राक्षसी वृत्ति वाले और अदिव्य प्राणी हैं। राक्षस तामसिक होने । और असुर राजसिक । प्रकृति का अर्थ यहाँ स्वभाव से है।
वे केवल बाह्य, मानव शरीर को देखते हैं। भीतर विद्यमान आत्म तत्व से वे सर्वथा अनभिज्ञ हैं। विश्व में वे परमात्मा को नहीं देखते । मात्र क्षुधा-पिपासा को शान्त करने हेतु वे जीवन यापन करते हैं।
परमात्मा की कृपा के बिना जो केवल कर्म द्वारा ही प्रतिफल अवका पुरस्कार की आशा करते हैं वे व्यर्थ की आशा और व्यर्थ ही कर्म करते हैं। कर्म से जड़ है, वह स्वतन्त्र रूप से प्रतिफल नहीं दे सकता । सर्वज्ञ भगवान् ही उनका विधायक है जो कर्म और उसके प्रतिफल को जानने वाला है। जिन्होंने ऐसी पुस्तकों से ज्ञान अर्जित किया है जो न तो आत्मिक सत्ता को स्वीकारती हैं न ही उनमें आध्यात्मिक ज्ञान है वे मनुष्य व्यर्थ के ज्ञान से युक्त हैं। इससे कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मज्ञान से युक्त आध्यात्मिक पुस्तकों अथवा धर्म ग्रन्थों का अध्ययन ही वास्तविक फल दे सकता है। (निरूपण - VILIS; XVI.6, 20)
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ।।१३ ।।
शब्दार्थ : महात्मानः महान् आत्माएँ, तु-लेकिन, माम् -मुझे, मेरी, पार्थ-हे अर्जुन, दैवीम् -दिव्य, प्रकृतिम् -प्रकृति को, आश्रिताः- आश्रित, भजन्ति-पूजा करते हैं, अनन्यमनसः- अनन्य मन से, ज्ञात्वा-जान कर, भूतादिम् - जीवों के स्रोत को, अव्ययम् - अविनाशी ।
अनुवाद : किन्तु हे अर्जुन, महात्मा जन मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित हो कर, समस्त प्राणियों के अविनाशी उद्धव स्रोत रूप में मुझे जान कर अनन्या मन से (एकाग्र मन से) मेरी आराधना करते हैं।
व्याख्या : ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् - एक और व्याख्या है-मुझे सब भूतो का अर्थात् पंचभूतों और प्राणियों का मूल स्रोत और अविनाशी जान कर ।
दैवीं प्रकृतिम् - दैवी अथवा सात्त्विक प्रकृति । जो दिव्य प्रकृति से एक है और संयम, दया, निष्ठा और पवित्रता आदि गुणों से सम्पन्न है।
महात्मानः- महान् आत्माएँ वे हैं जिनके हृदय मेरे द्वारा विशेष रूप से श्री बास स्थान रूप में बनाये गये हैं। महात्माओं के विशुद्ध हृदयों में मैं वास करता हूँ। वे मेरे प्रति अचल भक्ति भाव रखते हैं। सात्त्विक प्रकृति, शुद्ध हृदय और आत्म ज्ञान से युक्त पुरुष महात्मा हैं।
भूतादि-समस्त जीव और पाँच तत्त्व ।
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ।।१४ ।।
शब्दार्थ : सततम् -सदा, कीर्तयन्तः- महिमा गाते हुए, माम् -मुझे, यतन्न्तः- यत्न करते हुए, च-और, दृढव्रताः- दृढ संकल्प वाले, नमस्यन्तः -प्रणाम करते हुए, च-और, माम् -मुझे, मेरी, भक्त्या -भक्ति भाव से, नित्ययुक्ताः सदा स्थिर (दृढ़ निश्चय वाले), उपासते -उपासना करते हैं।
अनुवाद : सतत मेरा कीर्तन (गुणगान) करते हुए, मेरे लिए यत्न करते हुए, दृढ़ संकल्प से युक्त, मुझे प्रणाम करते हुए वे नित्ययुक्त भक्तिभाव से मेरी उपासना करते हैं।
व्याख्या : ये महात्मा मेरा गुणगान करते हैं। वे ॐ का जप करते हैं। वे शास्त्राध्ययन करते हैं और उपनिषदों का पाठ करते हैं। वे अपने आध्यात्मिक गुरु से श्रुतियों (वेदों) का श्रवण करते हैं, उन पर चिन्तन-मनन करते हैं और निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वे पवित्रता, सत्य, सहनशीलता, प्रेम, दया और सहानुभूति आदि गुणों का विकास करते हैं। इन्द्रियों को वश में कर के मन को स्थिर करते हैं।
मन, वचन और कर्म की पवित्रता, सत्य और अहिंसा आदि व्रतों का वे दृढतापूर्वक पालन करते हैं। अत्यन्त निष्ठा और भक्ति भाव से वे मेरी पूजा करते हैं। हृदय में निहित अन्तरात्मा के रूप में वे मेरी आराधना करते हैं। एक नवदीक्षित शिष्य भगवान् के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता, उसे अपने आध्यात्मिक गुरु की पहले पूजा करनी होगी और उसे ही ब्रह्मस्वरुप मानना होगा।
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ।।१५ ।।
शब्दार्थ : ज्ञानयज्ञेन ज्ञान यज्ञ के द्वारा, च-और, अपि-भी, अन्ये-अन्य, यजन्तः यज्ञ करते हुए, माम् मुझे, उपासते-पूजते है एकत्वेन अभिन्न भाव से, पृथक्त्वेन पृथक् भाव से, बहुधा अनेक रूप से, विश्वतोमुखम् -विराट्स्वरूप को।
अनुवाद : अन्य (ज्ञानी जन) ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं जो विराट् स्वरूप है, अभिन्न, पृथक् और विविध स्वरूप है।
व्याख्या : सर्वव्यापक मुझ एक और अनेक स्वरूप की अन्य ज्ञानी जन सब में आत्म दर्शन करते हुए, ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी ही उपासना करते हैं। सब स्वरूपों में वे भगवद्-दर्शन करते हैं और सब ध्वनियों में भगवन्नाम ही श्रवण करते हैं। वे जो कुछ भी खाते हैं विभिन्न प्रकार से मुझे ही अर्पित करते हैं।
अन्य कुछ उसकी इस ज्ञान से पूजा करते हैं कि सत्य एक परमात्मा ही है जो सत्-चित्-आनन्द (सच्चिदानन्द) स्वरूप है। वे ब्रह्म के साथ एकत्व स्थापित करते हैं। यह वेदान्तियों का एक ईश्वरवाद है। कुछ अन्य पृथक् भाव से जैसे स्वामी और सेवक के भाव में उसकी आराधना करते हैं। द्वैतवाद अथवा दर्शन में द्वैत दर्शन यही है। अन्य ज्ञानी उसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव आदि देवों के रूप में वन्दन करते हैं।
विश्वतोमुखम् - अन्य जन उसके अनेक रूपों की कल्पना करके सब स्वरूपों में उसकी सत्ता को मान कर उसकी आराधना करते हैं। उनके अनुसार विभिन्न रूपों में सर्वतः मुख किये हुए वही विराजमान हैं। (निरूपण - IV.33)
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम् ।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ।।१६ ।।
शब्दार्थ : अहम् -मैं, क्रतुः अनुष्ठान, अहम् मैं, यज्ञः-यज्ञ, स्वधा स्वधा (पूर्वजों अथवा पितरों को तर्पण), अहम् -मैं, अहम् -मैं, औषधम्-औषधि (औषधीय गुण युक्त सभी जड़ें और पौधे), मन्त्रः-पावन अक्षर, अहम् -मैं, अहम् -मैं, एव-ही, आज्यम्-धी, अहम् - मैं, अग्नि:-अग्नि, अहम् -मैं, हुतम् आहुति ।
अनुवाद : क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि (जड़ी-बूटी और पोधे) मैं हूँ, मन्त्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, आहुति मैं हूँ।
व्याख्या : क्रतु एक प्रकार का वैदिक अनुष्ठान है। (श्रौत कर्म विशेष यज्ञ शंकर स्मार्त कर्म)
यज्ञ-धर्म शास्त्रों और स्मृति में निर्दिष्ट विधि-विधान सहित पूजा यज्ञ है। मन्त्र-गुणगान, जिसके द्वारा पितरों और देवों को आहुति दी जाती है। हुतम् -हवन की क्रिया ।
औषधम् -समस्त पौधे, जौ, चावल-धान आदि इसी श्रेणी में आते हैं अथवा वे औषधियाँ जो रोगहरण करती हैं। (सर्व प्राणिभिः यद् अद्यते तद् औषध शब्द वाच्यम् - शंकर) (निरूपण - IV.24)
पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ।।१७ ।।
शब्दार्थ : पिता-पिता, अहम् -मैं, अस्य-इस, जगतः- जगत् का, माता-माता, धाता-कर्म फल प्रदाता, पितामहः-पितामह (दादा), वेद्यम्-जानने योग्य, पवित्रम् -पवित्र, ओंकार:- ओंकार, ऋक्- ऋक्, साम-साम, यजुः यजुस्, एव-ही, च-और ।
अनुवाद : मैं इस विश्व का पिता हूँ, माता हूँ, कर्मफल प्रदाता हूँ और पितामह हूँ। मैं ज्ञातव्य (जानने योग्य) हूँ, पवित्र हूँ, पावन अक्षर ॐ हूँ, तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ।
व्याख्या : धाता-कर्मों का फल प्रदान करके पालन करने वाला। ईश्वर अथवा सगुण ब्रह्म पिता है। मूल प्रकृति माता है। पावन सच्चिदानन्द (सत्-चित्-आनन्द) पितामह हैं।
वेद्यम् -जानने योग्य एक ही तत्त्व है और वह है परमात्मा ।
पवित्रम् -पवित्र करने वाला। पावनी भागीरथी में स्नान सा मेरा स्वरूप है और गायत्री जप भी मेरा ही रूप है। ये दोनों साधकों की अन्तः शुद्धि करते हैं।
च-और, इसमें अथर्ववेद समाहित किया गया है। (निरूपण-XIV.3)
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ।। १८ ।।
शब्दार्थ : गतिः- लक्ष्य, भर्ता-पालनकर्ता, प्रभुः-स्वामी, साक्षी- (शुभाशुभ) देखने वाला, निवासः-निवास, शरणम् -शरण, सुहृत् -मित्र, प्रभवः-उद्भव, प्रलयः -प्रलय, स्थानम् -स्थान, निधानम् -कोषगृह, बीजम् - बीज, अव्ययम् अविनाशी ।
अनुवाद : मैं लक्ष्य (परम धाम), स्वामी, साक्षी, रहने योग्य निवास स्थान, सब का आश्रय, परम मित्र, उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, परम निधान और अविनाशी बीज (कारण) हूँ।
व्याख्या : मैं लक्ष्य हूँ, कर्म का प्रतिफल हूँ। पालन-पोषण करने वाला स्वामी हूँ। जीवों के शुभाशुभ कर्मों का साक्षी हूँ। मैं वह स्थान हूँ जहाँ सब प्राणी वास करते हैं। दुःखी का आश्रय मैं हूँ। शरणागत के दुःखहरण मैं ही करता हूँ। मैं वह सच्चा मित्र हूँ जो बदले में कुछ लेने के भाव को त्याग कर भला करता है। इस ब्रह्माण्ड का उद्भव मैं हूँ। मुझ में ही सम्पूर्ण जगत् लीन होता है। मैं ही संसार का आधार हूँ। मैं ही वह कोषगृह हूँ जिसे भविष्य में प्राणी उपभोग करेंगे। मैं अविनाशी बीज हूँ अर्थात् जीवों के उद्भव का कारण हूँ। अतः मेरे चरण-शरण में आ जाओ।
तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ।।१९ ।।
शब्दार्थ : तपामि -(मैं) उष्णता देता हूँ, अहम् -मैं, अहम् मैं, वर्षम् -वर्षा, निगृह्णामि-रोकता हूँ, उत्सृजामि-बरसाता हूँ, च-और, अमृतम्-अमृतत्व, च-और, एव-ही, मृत्युः- मृत्यु, च-और, सत्- अस्तित्व, असत् - अन्-अस्तित्व, च-और, अहम् -मैं, अर्जुन- हे अर्जुन ।
अनुवाद : (सूर्य रूप में) मैं उष्णता (ताप) देता हूँ, वर्षा का आकर्षण और वर्षण मैं ही करता हूँ। मैं ही अमृतत्व हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, हे अर्जुन, सत् और असत् भी मैं ही हूँ।
व्याख्या: सूर्य के ताप का प्रसार मैं करता हूँ। इन्द्र रूप से वर्षा ऋतु में वर्षा मैं करता हूँ, वर्ष के शेष काल इसका विकर्षण भी मैं ही करता हूँ।
सत्-अस्तित्व, व्यक्त सृष्टि (कार्य रूप)
असत् - अनस्तित्व, अव्यक्त (कारण रूप)
असत् का अभिप्राय 'कुछ नहीं' से अथवा शून्य नहीं है। सूक्ष्म, अव्यक्त कारण ही असत् कहलाता है। आत्मा, ब्रह्म अथवा शाश्वत, सर्वथा असत् नहीं हो सकते। उनकी सत्ता सदा विद्यमान है। यह सत् स्वरूप है। यदि सूक्ष्म अव्यक्त कारण को शून्य माना जाये तो शून्य में से सृष्टि की अवधारणा करना असम्भव है। छान्दोग्योपनिषद् में वर्णन है- "असत् से सत् की सृष्टि कैसे सम्भव है?" असत् से सत् की सृष्टि का विचार करना मूर्खता है। एक वेदान्त के साधक के लिए ब्रह्म सत् है क्योंकि यह सदा विद्यमान और अपरिवर्तनशील (अविकारी) है। यह अभिव्यक्त सृष्टि असत् है, सांसारिक लोगों के लिए, जिनके पास न तो विवेक है न ब्रह्मज्ञान, जो अपवित्र स्थूल बुद्धि से युक्त हैं, जिनके पास प्रखर और सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, जो केवल स्थूल रूप ही देख सकते हैं, यह अभिव्यक्त संसार ही सत् है और सूक्ष्म अव्यक्त मूल प्रकृति जो अभिव्यक्त संसार का मूल कारण है, वह असत् है उनके लिए ब्रह्म भी असत् है। अव्यक्त का संकेत मूल प्रकृति और ब्रह्म दोनों की ओर है क्योंकि दोनों ही अप्रत्यक्ष हैं।
प्रत्येक पदार्थ की तीन अवस्थाएँ हैं-स्थूल, सूक्ष्म और कारण । महाकारण (जिसका कोई कारण नहीं) परब्रह्म है। स्थूल और सूक्ष्म अवस्थायें कारण के कार्य रूप (effects) हैं। बाहर जो प्रत्यक्ष है वह स्थूल शरीर है। यह भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर (वायवीय शरीर) से चलता है जो मन, प्राण और इन्द्रियों से निर्मित है। कारण शरीर बीज शरीर है। इसी बीज शरीर से सूक्ष्म और स्थूल शरीर उत्पन्न हुए हैं। एक सन्तरे का ही विचार करो। इसका बाह्य शरीर (बाह्य त्वचा) भौतिक शरीर है। अन्दर का गूदा अथवा सार सूक्ष्म शरीर है, किन्तु गूदा और बाहर की त्वचा को बनाने वाला अन्तस्तम कारण शरीर बीज है। यह एक स्थूल चित्रण है। सन्तरे के दूसरे प्रकार के सूक्ष्म और कारण शरीर हैं। सांसारिक मनुष्य केवल भौतिक शरीर देखता है और उसी को सत्य मानता है। उसके लिए सूक्ष्म (वायवीय) और कारण शरीर असत् है।
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ।।२० ।।
शब्दार्थ : त्रैविद्याः तीनों वेदों को जानने वाले, माम् -मुझे, सोमपाः सोमरस पीने वाले, पूतपापा:-पापों से मुक्त, यज्ञैः यज्ञों के द्वारा, इष्ट्वा-पूजा कर के, स्वर्गतिम् -स्वर्ग की, प्रार्थयन्ते-प्रार्थना करते हैं, ते-वे,पुण्यम् -पुण्य, आसाद्य-प्राप्त करके, सुरेन्द्रलोकम् - इन्द्रलोक को, अश्नन्ति- भोगते हैं, दिव्यान्-दिव्य, दिवि-स्वर्गलोक में, देवभोगान्दैवी भोगों को।
अनुवाद : तीनों वेदों का ज्ञान रखने वाले, सोमरस पान करने वाले, पापों से मुक्त हो कर, यजन द्वारा मेरी पूजा करते हुए स्वर्ग लोक के लिए प्रार्थना करते हैं। वे देवताओं के ईश इन्द्र के पावन स्वर्ग लोक को प्राप्त कर वहाँ देवताओं के दिव्य सुखों का भोग करते हैं।
व्याख्या : अनेक साधक योग के सोपान पर एक विशेष ऊँचाई तक आरूढ़ होते हैं। उच्चतर लोक से आकृष्ट हो कर मोहित हुए से वे अनियंत्रित रूप से खिंचे चले जाते हैं। विवेक शक्ति और सम्यक् बोध को खो कर वे स्वर्गिक भोगों में स्वयं को भी भूल जाते हैं। उच्चतर लोक (स्वर्ग) में वास करने वाले दिव्य देव विभिन्न प्रकार से साधक को आकृष्ट करते हैं। वे उन्हें कहते हैं-"हे योगी, हम तुम्हारी तपश्चर्या और विरक्त भाव, आध्यात्मिक अभ्यास और दिव्य गुणों से अतीव प्रसन्न हैं। अपनी तपस्या और गुणों से प्राप्त किया गया यह लोक तुम्हारा अन्तिम आश्रयस्थल (परम धाम) है। तुम्हारे आदेश, तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए हम तुम्हारे सेवक हैं। यह लो तुम्हारे लिए दिव्य वाहन । कहीं भी भ्रमण करना चाहो करो। तुम्हारी सेवा में ये रहीं दिव्याङ्गनायें, वे दिव्य संगीत से तुम्हारा प्रमोद करेंगी। यह रहा कल्पवृक्ष जो तुम्हें आकांक्षित फल प्रदान करेगा। स्वर्ण पात्र में यह लो अमृत जो तुम्हें अमर कर देगा। यह है दिव्य झील (सरोवर), परम आनन्द को देने वाली, तुम स्वतन्त्रता पूर्वक इसमें तैर सकते हो।" असावधान योगी देवताओं के निमन्त्रण और मधुर पुष्पित वाणी से सहज ही आकृष्ट हो जाता है। उसे मिथ्या सन्तोष की प्राप्ति होती है। वह सोचता है कि वह योग के अन्तिम सोपान पर आ चुका है। वह उन आकर्षणों में फंस जाता है और उसकी शक्ति विभिन्न दिशाओं में विकीर्ण हो जाती है (बिखर जाती है) । जैसे ही उसके पुण्य क्षीण होते हैं वह पुनः मर्त्य लोक में आ जाता है। अब पुनः आध्यात्मिक सोपान पर चढ़ने के लिए उसे एक बार पुनः प्रयास करना पड़ेगा। किन्तु एक अनासक्त योगी जो प्रबल विवेक से युक्त है, देवताओं के निमन्त्रण को निर्दयतापूर्वक ठुकरा देता है, अपने आध्यात्मिक पथ पर निर्भीकता से आगे बढ़ता है ओर योग के अन्तिम सोपान अथवा ज्ञान के सर्वोच्च शिखर अथवा निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त होने तक नहीं रुकता । वह पूर्णतया सचेत होता है कि स्वर्ग लोक के भोग उतने ही मूल्य हीन हैं जितने इस मिथ्या मर्त्य लोक के। स्वर्गिक सुख सूक्ष्म हैं, अत्यन्त श्रेष्ठ और पराकोटि के हैं, मोहित करने वाले हैं। यही कारण है कि थोड़ा सा भी असावधान, अजागरूक और अल्प अनासक्त साधक उच्चतर स्वर्गिक लोक के सुखों से सुगमतापूर्वक आकृष्ट हो जाता है। इस भौतिक जगत् के पाश्चात्य देशों और अमेरिका में, जहाँ धन की प्रचुरता है, डालर और स्वर्ण का अभाव नहीं है, वहाँ लोग सूक्ष्म और उत्कट इन्द्रिय सुखों के भोगों में मस्त हैं। प्रतिदिन वैज्ञानिक नई-नई खोज करते हैं। आक्रामक और अनिष्टकारी शरारती इन्द्रियों की सन्तुष्टि के लिए नये-नये सुख साधनों का अन्वेषण करते हैं। अमेरिका अथवा योरोप में वास करने के उपरान्त एक सामान्य सरल संयत भारतीय भी परिवर्तित व्यक्ति प्रतीत होता है। वह आकर्षणों से मुग्ध हो उठता है। माया की ऐसी महान् शक्ति है। आकर्षणों का ऐसा प्रभाव है। इन्द्रियाँ इतनी प्रबल हैं। दृढ़ संकल्प और विवेक से युक्त, संयत, अनासक्त, अच्छी आत्म-विश्लेषण की शक्ति से युक्त और मोक्ष की ज्वलन्त आकांक्षा से युक्त पुरुष ही आकर्षणों पर संयम रख सकता है और केवल वही सुखी हो सकता है। जीवन के अन्तिम लक्ष्य सर्वोच्च आनन्द और अनन्त की उत्कृष्ट दिव्य दृष्टि वही प्राप्त कर सकता है।
सोमरस का पान करने वाले पाप मुक्त हो जाते हैं।
यज्ञैः-अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ ।
अग्निष्टोम आदि यज्ञों से वे वसु, रुद्र, आदित्य आदि देवताओं के रूप में मेरी आराधना करते हैं।
इन्द्र देवताओं का राजा है। उसे शतक्रतु कहते हैं क्योंकि उसने एक सौ यज्ञ किये थे। दिव्य सुख स्वर्ग के अलौकिक सुख हैं।
दिव्य भोग-दिव्य भोग मनुष्य की पहुँच से परे हैं। देवताओं के दिव्य शरीर ही इसका भोग कर सकते हैं। स्वर्ग में देवताओं द्वारा प्रदत्त भोग दिव्य भोग है। भोग का संकेत इन्द्रिय सुख भोग की ओर है। यद्यपि स्वर्ग के भोग अत्यन्त
सूक्ष्म प्रकृति के हैं तथापि वे केवल इन्द्रिय भोग ही हैं। (निरूपण -11.45)
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं कामकामा लभन्ते ।।२१ ।।
शब्दार्थ : ते-वे, तम्-उसे, भुक्त्वा-भोग कर, स्वर्गलोकम् -स्वर्ग लोक को, विशालम् - विशाल, क्षीणे - क्षीण होने पर (समाप्त होने पर), पुण्ये-पुण्य कर्म, मर्त्यलोकम् -मृत्यु लोक को, विशन्ति-प्रवेश करते हैं, एवम् - इस प्रकार, त्रयीधर्मम् तीनों वेदों के धर्म का, अनुप्रपन्नाः-पालन करने वाले, गतागतम् आवागमन की अवस्था में, कामकामा:-इच्छाओं की इच्छा करते हुए, लभन्ते-प्राप्त करते हैं।
अनुवाद : विशाल स्वर्ग लोक का सुख भोग कर वे पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक (भू लोक) में पुनः लौटते हैं। एवंविध, वेदत्रयी के आदेशों का पालन करते हुए, विषयों की कामना करते हुए वे (साधक) आवागमन की अवस्था को प्राप्त होते हैं।
व्याख्या : (स्वर्गिक सुखों का कारण) संचित पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाते हैं वे इस लोक में अवरोहण करते हैं। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें कोई अपनी स्वतन्त्रता नहीं है।
त्रयीधर्म-तीनों बेटों से सम्बद्ध वैदिक अनुष्ठान ।
कामकामा:-वे लोग, जिनके मन सांसारिक वासनाओं से भरे हुए हैं।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।।२२ ।।
शब्दार्थ : अनन्याः-अनन्यभाव से, चिन्तयन्तः - विचार करते हुए, माम्-मुझे, ये-जो, जनाः लोग, पर्युपासते -पूजते हैं, तेषाम् - उनका, सिमाभियुक्तानाम् - नित्ययुक्त, योगक्षेमम् - योग और क्षेम (अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा), वहामि-वहन करता हूँ, अहम् -मैं।
अनुवाद : अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करने वाले और मेरी ही आराधना करने वाले नित्ययुक्त साधकों का योग-क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ।
व्याख्या : अनन्यः - अभिन्न । यह एक और अर्थ है। मेरा ध्यान करते हुए जो लोग समस्त प्राणियों में मेरी पूजा करते हैं ऐसे नित्य ही भक्तिभाव में लीन लोगों का योग-क्षेम (लाभ और रक्षा) मैं वहन करता हूँ। वे स्वयं को, अपने आत्म तत्त्व को, परम सत्ता से अभिन्न मानते हैं। वे परम-पुरुष का अपनी ही आत्मा में दर्शन करते हैं।
ऐसे भक्त जो अपने आत्म तत्त्व से पृथक् किसी को नहीं देखते और समदृष्टि रखते हैं उनका अपना स्वार्थ कोई नहीं होता। वे अपने ही लाभ और सुरक्षा का चिन्तन नहीं करते । उन्हें जन्म-मृत्यु की कोई कामना नहीं होती । उनके पास खोने को कुछ नहीं होता क्योंकि अपना कहने योग्य उनके पास कुछ है ही नहीं। उनके तो शरीर भी भगवान् के हो जाते हैं। कुछ प्राप्ति की उन्हें आकाङ्क्षा नहीं होती क्योंकि उनकी समस्त कामनायें भगवान् के साथ वार्तालाप से ही पूर्ण हो जाती हैं। भगवान् के परा सम्पदा और समस्त दिव्य ऐश्वर्य उनके पास होने के कारण वे सदा सन्तुष्ट रहते हैं।
भगवान् के अतिरिक्त कोई विचार स्वयं उनके मन में ही नहीं आता। परिणाम स्वरूप भगवान् स्वयं उनके दैहिक निर्वाह का ध्यान करते हैं और उन्हें वस्त्र, भोजन आदि का अभाव नहीं होता। इसे योग कहते हैं। उनके पास जो कुछ पहले से ही है उसकी वे रक्षा करते हैं और यह क्षेम कहलाता है। ये दोनों कार्य भगवान् करते हैं। माता-पिता जिस प्रकार अपने बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान करते हैं उसी प्रकार भगवान् अपने भक्तों के अभावों की पूर्ति करते हैं।
वे पूर्ण निष्ठा के साथ अपना समग्र मन भगवतोन्मुख करते हैं। केवल भगवान् को ही वे चिन्तन का विषय बनाते हैं। भगवान् से अधिक प्रियतर इस सम्पूर्ण विश्व में उनके लिए और कोई नहीं होता। वे तो भगवान् के लिए जीवन जीते हैं। एक ही उद्देश्य से और अनन्य भक्ति से वे भगवत् चिन्तन करते हैं। भगवान् के अतिरिक्त वे अन्य कुछ नहीं देखते । समस्त जीवों में वे भगवद्दर्शन करते हैं और उन्हें प्रेम करते हैं। वे जब ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं तो भगवान् भी उनके योग-क्षेम का भार अपने ऊपर ले लेते हैं।
नित्ययुक्त-वे हैं जो एकाग्र चित्त हो कर नितान्त भक्तिभाव से युक्त हो कर सतत भगवान् का ध्यान करते हैं। (निरूपण-VIII.14. XVIIII .66 )
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ।।२३ ।।
शब्दार्थ : ये-जो, अपि-भी, अन्यदेवताः- अन्य देव, भक्ताः- भक्त, यजन्ते-पूजा करते हैं, श्रद्धया -श्रद्धा भाव से, अन्विताः युक्त हो कर, ते-वे, अपि-भी, माम् -मुझे, एव-ही, कौन्तेय- हे कौन्तेय, यजन्ति-पूजते हैं, अविधिपूर्वकम् - विधि-विधान रहित, अज्ञानपूर्वक ।
अनुवाद : अन्य भक्तजन भी, हे अर्जुन, जो अन्य देवताओं की आराधना करते हैं वे वस्तुतः अविधिपूर्वक मेरी ही आराधना करते हैं।
व्याख्या : वे अज्ञानवश मेरी पूजा करते हैं। उनकी पूजा-विधि प्राचीन विधि-विधानों के विपरीत होती है। अतः मरणोपरान्त पुनः इसी संसार में जन्म लेकर लौट आते हैं।
अग्नि, इन्द्र, सूर्य, वरुण और वसु आदि की लोग पूजा करते हैं। वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं क्योंकि मैं तो सर्वत्र व्यापक हूँ किन्तु उनकी भक्ति पावन नहीं होती। यह दूसरों के लिए है। जल से मूल को सींचना अनिवार्य है, शाखाओं को नहीं। यदि मूल सन्तुष्ट है तो सम्पूर्ण वृक्ष सन्तुष्ट है और होना भी चाहिए। एवंविध, यदि मैं (जगत् का और देवताओं का मूल) सन्तुष्ट होता हूँ तो सारे देवता सन्तुष्ट होते हैं और होने चाहिए। यद्यपि पंच ज्ञानेन्द्रियों के संदेश एक ही चेतना को पहुँचते हैं तथापि, क्या यह उचित होगा कि मधु को कर्ण में, पुष्प को नेत्र में रखा जाये ? भक्षण का कार्य केवल मुख द्वारा ही होना चाहिए और घ्राण (सूंघने) का कार्य नासिका से होना चाहिए। अतः मेरी पूजा मेरे ही नाम से होनी चाहिए। साधक और भक्त मुझे सब प्राणियों की आत्मा रूप से जानें। वे मुझे देवताओं का और जगत् का मूल कारण हूँ। (निरूपण- IV.11; VII.20)
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात श्श्यवन्ति ते ।।२४ ।।
शब्दार्थ : अहम् -मैं, हि-निश्चित रूप से, सर्वयज्ञानाम् -सब यज्ञों का, भोक्ता-भोग करने वाला, चऔर, प्रभुः स्वामी, एव-ही, च-और, न नहीं, दु-किन्तु, माम् -मुझे, अभिजानन्ति जानते हैं, तत्त्वेन तत्त्व से, अतः इसलिए, च्यवन्ति-गिरते हैं, ते-वे।
अनुवाद : समस्त यज्ञों का स्वामी और भोक्ता केवल मैं ही हूँ। किन्तु वे तत्व रूप से मुझे नहीं जानते और इसीलिए वे गिरते हैं (मर्त्यलोक में पुनर्जन्म लेते हैं)।
व्याख्या : वे नहीं जानते कि वेदों और स्मृतियों (आचार संहिता) में विहित सब यज्ञों का भोक्ता मैं परम पुरुष ही हूँ और समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ। संसार का अन्तः शासक होने के कारण मैं ही यज्ञों का स्वामी हूँ, (अधियज्ञोऽहमेवात्र, VIII.4) मैं ही यज्ञों का अधिष्ठातृ देव हूँ। यज्ञ के प्रारम्भ में भी मैं ही हूँ और अन्त में भी मैं ही हूँ। फिर भी ये लोग अन्य देवों की पूजा करते हैं। अतः वे अज्ञान में पूजा करते हैं। अन्य देवताओं की पूजा करते समय वे मेरा अभिज्ञान नहीं कर पाते और क्योंकि वे अपने कर्म भी मुझे समर्पित नहीं करते इसीलिए जिस प्रयोजन से उन्होंने वे शुभ कर्म यज्ञादि किये थे उस का फल भोग कर पुण्य समाप्त होने पर पुनः इस मर्त्य लोक में लौट आते हैं।
जो लोग अन्य देवों में आसक्त हैं और अज्ञान में मेरी पूजा करते हैं (अविधिपूर्वकम्) वे भी अनुष्ठान का फल प्राप्त करते हैं। कैसे? (निरूपण-V.29.XV.9)
यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ।। २५ ।।
शब्दार्थ : यान्ति-प्राप्त होते हैं, देवव्रताः-देवताओं की पूजा करने वाले, देवान् -देवताओं को, पितृन् -पितरों को, यान्ति-जाते हैं, पितृव्रताः- पितरों की पूजा करने वाले, भूतानि-भूतों को, यान्ति-जाते हैं, भूतेज्याः - भूतों की पूजा करने बाले, यान्ति-जाते हैं, मद्याजिनः- मेरे आराधक, अपि-भी, माम् -मुझे ।
अनुवाद : देवताओं को पूजने वाले देवताओं को जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले पंचभूतों के अधिष्ठातृ देवों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं।
व्याख्या : अग्निष्वत्त (Agnisvattas) आदि पितरों के पुजारी जो पितृ भक्ति में श्राद्ध आदि अनुष्ठान करते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं। संकल्प और भक्तिसहित देव पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं।
भूत तत्त्वों से सम्बद्ध प्राणी हैं जो देवताओं से तो निम्न हैं परन्तु मनुष्यों से ऊपर हैं, वे विनायक हैं, वे चार भगिनी आदि माताओं के आतिथेय (Hosts) हैं।
देवभक्ति में लीन व्यक्ति मृत्यु के समय उन्हीं देवताओं के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से पितरों को पूजने वाले और भूतों को पूजने वालों का भाग्य होता है। भक्त की पूजा की प्रकृति, दान, निष्ठा और ज्ञान के अनुरूप ही पूजा का परिणाम होता है।
यद्यपि संघर्ष और प्रयास तो समान ही हैं तथापि लोग अज्ञानवश मेरी पूजा नहीं करते। परिणामस्वरूप वे बहुत कम प्रतिफल प्राप्त करते हैं।
मेरे भक्तों को अनन्तफल की प्राप्ति होती है। वे इस भूलोक में पुनः नहीं आते। मेरी आराधना उनके लिए सहज भी है। कैसे ? (निरूपण-VII.23)
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ।।२६ ।।
शब्दार्थ : पत्रम् -पत्र (पत्ता), पुष्पम् -पुष्प, फलम् -फल, तोयम् जल, यः जो, मे-मुझे, भक्त्या-भक्ति भाव से, प्रयच्छति-अर्पण करता है, तत्वह, अहम् -मैं, भक्त्युपहतम् - भक्तिपूर्वक अर्पित, अश्नामि-स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ, प्रयतात्मनः- पवित्र मन वाले का।
अनुवाद : जो भी भक्त भक्तिभाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है, पवित्र मन से और भक्ति भाव से अर्पण की उस भेंट को मैं स्वीकार करता हूँ।
व्याख्या : पूर्ण निष्ठा से अर्पित की गई अल्प भेंट भी भगवान् को स्वीकार है। शुद्ध हृदय, एकाग्र मन से अर्पण किये गये पत्र, पुष्प, फल और जल से भी भगवान् अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं। शबरी के बेर और सुदामा की पोटली से थोड़े से धुने चावल स्वीकार कर के क्या वे सन्तुष्ट नहीं हुए थे? उनके लिए सैण-मन्दिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण-मन्दिर तो अपने हृदय में बनाओ। भगवान् को उसमें विराजित करो। भगवान् को तो केवल तुम्हारा भक्तिपूर्ण हृदय चाहिए। किन्तु इन्द्र को प्रसन्न करना कठिन है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो तुम्हें अमूल्य पदार्थ भेंट करने होंगे।
पत्र, पुष्प और फल तो मात्र संकेत हैं। भगवान् की प्राप्ति का सच्चा साधन पवित्र, अचल भक्ति है। राज्य के समस्त पदार्थ राजा की सम्पदा होते हैं किन्तु राज्य के सेवक यदि भक्तिभाव (प्रेमभाव) से राजा को कुछ उपहार देते हैं तो वह अति प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार विश्व की सम्पूर्ण सामग्री भगवान् की ही सम्पदा है पुनरपि प्रीतिपूर्वक यदि तुम उन्हें कुछ अर्पण करते हो तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं।
अश्नामि का अर्थ तो 'भक्षण' भाव में है किन्तु सांकेतिक अथवा लक्षणा वृत्ति में इसका अर्थ 'स्वीकार करना' है।
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ।।२७ ।।
शब्दार्थ : यत्-जो, करोषि-करते हो, यत्-जो (भी), अश्नासिखाते हो, यत्-जो, जुहोषि-हवन करते हो, ददासि - देते हो, यत्-जो, यत्-जो, तपस्यसि-तपस्या करते हो, कौन्तेय- हे कौन्तेय, तत्-वह, कुरुष्व-करो, मदर्पणम् -मेरे अर्पण ।
अनुवाद : हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान करते हो, जो तपस्या करते हो वह सब मेरे अर्पण कर दो।
व्याख्या : सारे कर्म भगवान् को समर्पित कर दो। तभी कर्म बन्धन से मुक्ति पाओगे। कर्म की स्वतन्त्रता प्राप्त करोगे। इस श्लोक के भाव में तल्लीन रहने का अभ्यास करने वाला साधक भगवान् के प्रति आत्मसमर्पण के योग्य हो जाता है। धीरे-धीरे वह एक-एक कर के आध्यात्मिक सोपानों का आरोहण करता है। उसकी लोभ-वृत्ति अब पूर्णतः लुप्त हो चुकती है। वह सदा दान करता है। लेने की अभिलाषा उसमें नहीं रहती। अन्ततोगत्वा, उसका सम्पूर्ण जीवन विचार, भाव सहित भगवान् के चरणों में समर्पित हो जाता है। वह भगवान् के लिए ही जीता है। भगवान् के लिए ही कार्य करता है। अहंभाव पूर्णतया नष्ट हो जाता है। उसकी समस्त प्रकृति दिव्यता में परिवर्तित हो जाती है। कर्म जब भगवान् को समर्पित हो गये तो पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता। योग का यह सरलतम साधन है। अब और अधिक समय व्यर्थ न करो। आज से ही (योग) प्रारम्भ करो।
समस्त कर्म, समस्त परिणाम और समस्त प्रतिफल अथवा दान भगवान को ही पहुँचते हैं। व्यक्ति के लिए अपना पृथक् जीवन कुछ भी नहीं है। अपना नाम और रूप त्याग कर जिस प्रकार नदी सागर में जा मिलती है उसी प्रकार जीवात्मा अपना नाम, रूप अहंभाव और अहंता से युक्त इच्छाओं को त्याग कर परम पुरुष में जा मिलता है। व्यष्टि इच्छा समष्टि इच्छा से एक हो जाती है। अपनी मनोहारी इच्छा से जो कुछ भी तुम करते हो, शास्त्रविधि के अनुरूप जो भी यज्ञ में अर्पण करते हो, स्वर्ण, धान, घृत, वस्त्र आदि जो कुछ भी दान करते हो (ब्राह्मणों को अथवा लोगों को), पाप नाश के लिए चान्द्रायण व्रत, इन्द्रिय संयम आदि जो भी तपस्या करते हो-ये सब मुझे समर्पित करते हुए करो। (निरूपण - V.32; XII.6,8)
इस प्रकार तुम्हें क्या प्राप्ति होगी, उसे सुनो।
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ।
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।।२८ ।।
शब्दार्थ : शुभाशुभफलैः-शुभ और अशुभ फल से, एवम् - इस प्रकार, मोक्ष्यसे मुक्त हो जाओगे, कर्मबन्धनैः-कर्मों के बन्धन से, संन्यासयोगयुक्तात्मा-संन्यास योग से युक्त मन से, विमुक्तः - मुक्त, माम् -मुझे, उपैष्यसि प्राप्त करोगे ।
अनुवाद : इस प्रकार अनन्य मन से संन्यास योग में युक्त हो कर तुम भाशुभ (अच्छे बुरे) कर्मों के फल और कर्मों से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष प्त करके मुझे प्राप्त हो ओगे।
व्याख्या : एवम् - इस प्रकार अर्थात् जब तुम सर्वस्व मेरे अर्पण कर दो।
समस्त कर्मफल का त्याग संन्यास है। संन्यास योग से जिसका मन सज्जित है वह संन्यासयोगयुक्तात्मा है। सर्वस्व समर्पण की प्रक्रिया संन्यास योग है। यह योग भी है क्योंकि यह कर्म है। संन्यास और योग से युक्त मन के द्वारा तुम जीवनकाल में ही शुभाशुभ कर्म फल से मुक्त हो जाओगे और शरीर शान्त होने पर मुझे प्राप्त करोगे। एक आलोचक का कथन है- "फिर तो भगवान् भी प्रेम और घृणा के आधीन हैं क्योंकि वे अपने भक्तों पर ही कृपा वृष्टि करते हैं अन्यों पर नहीं।"
उत्तर है-ऐसा नहीं है। भगवान् तो पक्षपात रहित हैं और घृणा और प्रेम से अतीत हैं। उनकी कृपा सब के लिए प्रवाहित हो रही है किन्तु भक्त ही स्वतन्त्रता से इसे प्राप्त करता है क्योंकि कृपा प्राप्त करने के लिए उसने अपने हृदय के द्वार खोल रखे हैं।
इसकी व्याख्या अगले श्लोक में है।
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ।।२९ ।।
शब्दार्थ : समः समान, अहम् -मैं, सर्वभूतेषु सब प्राणियों में, न-नहीं, मे-मुझे, द्वेष्यः-घृणा का पात्र, अस्ति-है, न-नहीं, प्रियः-प्रिय, दे-जो, भजन्ति-पूजा करते हैं, तु-परन्तु, माम्-मेरी, भक्त्या-भक्तिभाव, मयि-मुझ में, ते-वे, तेषु उनमें, च-और, अपि-भी, अहम् -मैं।
अनुवाद : मैं सब प्राणियों के लिए समान हूँ, न तो कोई मुझे अप्रिय है और न ही प्रिय, किन्तु वे जो भक्तिभाव से मेरा अर्चन-पूजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ।
व्याख्या : भगवान् समदृष्टि हैं। वे सब प्राणियों को समदृष्टि से देखते हैं। न तो वे किसी की उपेक्षा करते हैं और न ही किसी से अपेक्षा रखते हैं। वे किसी के शत्रु नहीं हैं। किसी के पक्षपाती प्रेमी नहीं हैं। वे किसी के लिए पक्ष सेते हों और किसी पर क्रोध करते हों, ऐसा नहीं है। अहंकारी मनुष्य ही अपने दुर्व्यवहार से अपने और भगवान् के बीच दूरी कर लेता है। भगवान् तो उसके अपने श्वास और हाथ-पैर से भी अधिक उसके निकट हैं।
मैं तो अग्नि स्वरूप हूँ। जो अग्नि के निकट आते हैं वे शीत से बच जाते हैं किन्तु अग्नि से दूर रहने वाले यह लाभ नहीं ले सकते। उसी प्रकार मैं अपने भक्तों पर कृपा वृष्टि करता हूँ किसी आसक्ति वश नहीं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी स्वच्छ निर्मल दर्पण में ही प्रतिबिम्बित हो सकता है पात्र में नहीं उसी प्रकार सर्वव्यापक मैं परम पुरुष उन भक्तों के हृदयों में प्रकट होता हूँ जो सब प्रकार की (अज्ञान रूपी) अपवित्रता से भक्ति के द्वारा परिष्कृत हो चुके हैं।
सूर्य को न तो दर्पण से आसक्ति है न पात्र से घृणा । कल्प वृक्ष को लोगों के लिए प्रेम और घृणा नहीं होती किन्तु इच्छित पदार्थ तो उसे ही प्राप्त होंगे जो उसके समीप जायेगा। (निरूपण - VII.17; XII.14, 20)
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।। ३० ।।
शब्दार्थ : अपि - (भी) यद्यपि, चेत्-यदि, सुदुराचारः अत्यन्त दुराचारी, भजते-भजता है, माम् -मुझे, अनन्यभाक् -किसी अन्य के प्रति भक्ति न रखते हुए (अनन्य भाव से), साधुः साधु, एव-ही, सः- वह, मन्तव्यः - माना जाना चाहिए, सम्यक् यथार्थ निश्चय वाला, व्यवसितः - दृढ़ संकल्प वाला, हि-निश्चित रूप से, सः वह ।
अनुवाद : अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मेरी आराधना करता है तो वह साधु ही कहलाने योग्य है क्यों कि उसने सम्यक् निश्चय (मेरे भजन का) कर लिया है।
व्याख्या : अत्यन्त पापी भी यदि भगवान् का भजन करता है तो वह अच्छा ही कहा जाना चाहिए क्योंकि उसने दुराचार त्यागने का पावन संकल्प ले लिया है। डाकू रत्नाकर अपने अच्छे संकल्प से वाल्मीकि बन गया। जगाई और मधाई (Jagai & Madhai) भी धर्म भक्त हो गए। मेरी मैग्डलीन (Mary Magdalene) जो कुख्यात नारी थी, आदर्श नारी बन गई। हृदय में भगवान् का विचार आते ही पाप लुप्त हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। चान्द्रायण और कृच्छ व्रत कुछ विशेष पापों को ही नष्ट करेंगे किन्तु भगवन्नाम, परम पुरुष के विचार, जप, ध्यान और अभेद ब्रह्म चिन्तन (अद्वैत ब्रह्म का विचार अथवा अहं ब्रह्मास्मि) शत कोटि कल्पों में भी किये गये समस्त पापों को नष्ट कर देता है।
बाह्य जीवन में बुराई का मार्ग त्याग कर और अन्तर्मन से सम्यक् संकल्प के द्वारा साधक साधु बन जाता है और शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता है। (निरूपण-IV.36)
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।।३१ ।।
शब्दार्थ : क्षिप्रम् - शीघ्र, भवति-होता है, धर्मात्मा-धर्मात्मा, शश्वत् - नित्य, शान्तिम् - शान्ति, निगच्छति - प्राप्त करता है, कौन्तेय-कुन्ति पुत्र, प्रतिजानीहि-निश्चित जानो, न-नहीं, मेमेरा, भक्तः - भक्त, प्रणश्यति नष्ट होता है।
अनुवाद : वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो कर शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।
व्याख्या : सुनो, यह सत्य है, अर्जुन, तुम यह घोषणा कर सकते हो कि मेरे प्रति अनन्य भक्तिभाव वाला व्यक्ति जिसने अपना अन्तर्मन मुझे समर्पित कर दिया है, कभी नष्ट नहीं होता।
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ।।३२ ।।
शब्दार्थ : माम् -मुझे (मेरी), हि-निश्चित रूप से, पार्थ-हे पार्थ, व्यपाश्रित्य शरण में आ कर, ये-जो, अपि-भी, स्युः- हों, पापयोनयः- पाप-योनियाँ, स्त्रियः-स्त्रियाँ, वैश्याः- वैश्य, तथा-और, शूद्राः शूद्र, ते-वे, अपि-भी, यान्ति-प्राप्त करते हैं, पराम् -परम, गतिम् लक्ष्य को ।
अनुवाद : हे अर्जुन, मेरी शरण में आ कर पाप योनियों वाले स्त्री, वैश्य, शूद्र भी परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं।
व्याख्या : चाण्डाल और निम्न जाति के लोग पाप योनियों के हैं। सामाजिक नियमों के अन्तर्गत स्त्री और शूद्र वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं हैं। किन्तु भक्ति आकांक्षित है। पारिवारिक परम्पराओं की कोई आवश्यकता नहीं है। गजेन्द्र हाथी ने मुझे स्मरण किया और पशु होते हुए भी मुझे प्राप्त किया। निम्न से निम्नतर और दुष्ट से दुष्टतर भी मुझे प्राप्त कर सकता है यदि पूर्ण निष्ठा और विश्वास से वे मेरे नाम का जप करें, मेरा चिन्तन करें और किसी अन्य विषय का चिन्तन न करें। प्रह्लाद राक्षस जाति का था फिर भी मुझे उसके लिए नृसिंह अवतार लेना पड़ा। जन्म की महत्ता नहीं भक्ति ही सर्वस्व है, गोपियों ने अपनी भक्ति से मुझे प्राप्त किया। कंस और रावण ने भय से मुझे पाया। शिशुपाल ने घृणा से मुझे प्राप्त किया। नारद, ध्रुव, अक्रूर, शुक, सनत्कुमार और अन्यों ने मुझे भक्ति से प्राप्त किया। दक्षिण भारत में चिदम्बरम् में एक निम्न जाति के व्यक्ति नन्दन ने, जो भगवान् शिव का अनन्य भक्त था, भगवान् के प्रत्यक्ष दर्शन किये। आध्यात्मिक जीवन में सब जाति, मत, वर्ण-भेद सर्वथा लुप्त हो जाते हैं। शबरी, भीलनी होते हुए भगवान् की परम भक्त थी।
भारतीय धर्मशास्त्र इन घटनाओं से भरे पड़े हैं। हिन्दू धर्म में मोक्ष किसी विशेष मानव समुदाय तक सीमित नहीं है। भक्ति भाव हो तो सब को भगवत्-प्राप्ति का अधिकार है।
किं पुनर्बाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ।। ३३ ।।
शब्दार्थ : किम् पुनः-और कितना, ब्राह्मणाः - ब्राह्मण, पुण्याः-पुण्य, भक्ताः - भक्त, राजर्षयः राजर्षि, तथा-भी, अनित्यम् - अनित्य, असुखम् - असुख, लोकम्-लोक, इमम् - यह, प्राप्य - प्राप्त कर के, भजस्व-पूजा करो, माम् मेरी।
अनुवाद : और कितना (सहज रूप से) ब्राह्मण और राजर्षि भक्त लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस दुःखद क्षणभङ्गुर लोक को प्राप्त कर के अब तुम मेरी आराधना करो।
व्याख्या : राजर्षि वे राजा हैं जो राज्य पालन की अवधि में सन्त बन गये।
जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का मुख्य साधन यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। यह मानव शरीर पा कर तुम्हें भगवान् की भक्ति में जीवन व्यतीत करना चाहिए। केवल मानव शरीर में ही विचार शक्ति होती है, विवेक शक्ति और अनासक्ति होती है। देवताओं को भी इस मानव शरीर से ईर्ष्या होती है। यह शरीर अनित्य है। शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। यह विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं का घर है। अतः इस शरीर के लिए विश्राम और सुख प्राप्त करने के लिए संघर्ष छोड़ो । यह तन पाकर भी यदि तुम आत्म-साक्षात्कार को लक्ष्य नहीं बनाते तो तुम व्यर्थ ही जीते हो। तुम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो और आत्म हनन कर रहे हो। आवागमन के चक्र में पुनः-पुनः आओगे।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ।।३४ ।।
शब्दार्थ : मन्मनाः मुझ में मन वाला, भव-होओ, मद्भक्तः - मेरा भक्त, मद्याजी-मुझे अर्पित करते हुए, माम् -मुझे, नमस्कुरु-प्रणाम करो, माम् -मुझे, एव-ही, एष्यसि प्राप्त करोगे, युक्त्वा-युक्त हो कर, एवम् - इस प्रकार, आत्मानम् - आत्मा को, मत्परायणः- मुझे परम लक्ष्य मानते हुए।
अनुवाद : अपना मन मुझ में एकाग्र करो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यजन करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार पूर्ण मन से मेरे परायण हो कर मुझे ही अपना लक्ष्य मान कर तुम मुझे प्राप्त करोगे।
व्याख्या : मेरे भाव से मन पूर्ण करो। अपना मस्तिष्क, हृदय और हाथ मुझ में एकाग्र करो। मेरे सम-स्वरित बनो। सच्चे आराधक बनो। तुम शाश्वत शान्ति प्राप्त करोगे। मुझे जान कर तुम मृत्यु को जीत लोगे ।
बिना किसी आरक्षण के अपना सम्पूर्ण अस्तित्व भगवान् को समर्पित करो। तब सम्पूर्ण जीवन एक अद्भुत रूप में परिवर्तित होगा। सर्वत्र भगवान् के दर्शन करोगे।
समस्त दुःख और पीड़ाओं से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन दिव्य चेतना के साथ एक रूप हो जाएगा।
घट के टूटने पर जैसे घटाकाश (घट का आकाश) महदाकाश (ब्रह्माण्डीय आकाश) में मिल जाता है, गंगा और यमुना जैसे अपना नाम और रूप त्याग कर सागर *लीन हो जाती हैं उसी प्रकार प्रत्यक्ष आत्म दर्शन के द्वारा ज्ञानी सब प्रकार के सीमित प्रतिबंधकों (limiting adjuncts) से मुक्त हो कर पर ब्रह्म के साथ एकत्व स्थापित कर लेता है।
युक्त्वा का अभिप्राय है-विचार में स्थिर । इस प्रकार भगवान् में चित को स्थिर कर के, मुझे ही परम लक्ष्य और सर्वभूतात्मा मान कर मुझे ही प्राप्त होगा। (निरूपण-V.17; VII.7,14; XVIII.65)
इस अध्याय को अध्यात्म योग भी कहते हैं।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ।।
।। इति राजविद्याराजगुह्ययोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ दशमोऽध्यायः
विभूतियोगः
श्री भगवानुवाच
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।।१ ।।
शब्दार्थ : भूयः- पुनः, एव-ही, महाबाहो-हे महाबाहो (अर्जुन), सुनो, मे मेरा, परमम् परम, वचः वचन, यत्-जो, ते तुम्हारे लिए, कविता की सीममा सग-प्रिय के लिए, वक्ष्यामि कहूँगा, हितकाम्या (तु हिलर) कल्याण
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : पुनरपि, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम (रहस्य मय) वचन को सुनो जो मैं तुझ प्रिय के कल्याण की कामना से कहूँगा।
व्याख्या : मैं (७वें और ९वें अध्याय में) अपने कहे हुए वचनों की पुनरावृत्ति करूँगा। मेरी मूल प्रकृति और अभिव्यक्तियों का वर्णन तो पहले ही हो चुका है। मेरे दिव्य स्वभाव को समझना अत्यन्त कठिन है, यद्यपि इस विषय में मैं पूर्वतः ही कह चुका हूँ पुनरपि एक बार और इस विषय में कहूँगा। मैं अपनी दिव्य विभूतियों का उपदेश कर के तुम्हें चिन्तन योग्य विभूति के लिए अभिप्रेरित करूँगा ।
मेरा उपदेश श्रवण कर के तुम्हें प्रसन्नता होती है इसलिए मैं तुम्हारे लिए उपदेश करूँगा। अब तुम्हारा मन मुझ में रमण करने लगा है।
भगवान् अर्जुन को प्रोत्साहित और हर्षित करना चाहते हैं अतः अर्जुन के बिना कहे ही स्वयं उपदेश के लिए आगे आते हैं।
परमं वचः-परम वचन । निरतिशय वस्तु (unsurpassed truth) अर्थात् ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला वचन परम बचन है। है अर्जुन, तुम मेर वचन से अतीव हर्षित हो मानो अमृत-पान कर रहे हो।
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः ।।२ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, मे मेरा, विदु-जानते हैं, सुरगणा:- देवगण, प्रभवम् उद्भव, न नहीं, महर्षयः महान् ऋषि, अहम् मैं, आदि:-आदि, हि-क्योंकि, देवानाम् देवों का, महर्षीणाम् -महान् ऋषियों का, च-और, सर्वशः सब प्रकार से।
अनुवाद : न तो देवगण और न ही महर्षि गण मेरे उद्भव को जानते हैं क्योंकि सभी देवों और महर्षियों का स्रोत मैं ही हूँ।
व्याख्या : प्रभवम्-उत्पत्ति । इसका अभिप्राय 'भगवदीय कृपा' भी हो सकता है।
महर्षयः - भृगु आदि महान् ऋषि ।
समस्त प्राणियों, ऋषियों और देवों का मूल स्रोत मैं ही हूँ अतः उनके लिए मेरा ज्ञान प्राप्त करना दुष्कर है।
सर्वशः सब प्रकार से। सभी ऋषियों और देवताओं का मैं केवल उद्भव ही नहीं प्रत्युत् निमित्त कारण भी हूँ और उनकी बुद्धि आदि का पथ प्रदर्शक, स्वामी, प्रणेता और अन्तरात्मा भी मैं ही हूँ।
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।
असंमूढः स मर्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।३ ।।
शब्दार्थ : यः जो, माम्-मुझे, अजम्-अजन्मा, अनादिम् अनादि, च-और, वेत्ति -जानता है, लोकमहेश्वरम् - लोकों का स्वामी, असंमूढः- अभ्रमित ज्ञानवान), सः- वह, मर्त्यषु-मनुष्यों में, सर्वपापैः-सब पापों से, प्रमुच्यते -मुक्त जाता है।
अनुवाद : मनुष्यों में जो मुझे अनादि, अजन्मा और लोकों का महान् स्वामी मानता है वह ज्ञानवान् है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
व्याख्या : ब्रह्म ही सब लोकों का मूल कारण होने से वह अनादि है। महर्षियों और देवताओं का स्रोत होने के कारण उसकी निज सत्ता का कोई स्रोत नहीं है। वह अनादि है इसलिए जन्म रहित है और लोकों का शासक है।
असम्मूढः - भ्रम रहित । वही पुरुष ज्ञानी अथवा भ्रमरहित है जो अपनी अन्तरात्मा को परमात्मा से पृथक् नहीं समझता। अज्ञान का आवरण दूर होने से
आत्मा-अनात्मा का परस्पर अध्यारोपण भी दूर हो जाता है। चेतन-अचेतन अवस्था में किये गये तीनों कालों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं।
अज्ञानी मनुष्य प्रायश्चित्त कर्मों द्वारा अपने पापों का निराकरण करता है और प्रतिफल भोग कर पुण्य कर्मों को क्षीण करता है। किन्तु वह पापों से पूर्णतया मुक्त नहीं होता क्योंकि बुरे संस्कारों वश वह पाप कर्म करता ही रहता है और उसने पापों के मूल कारण अज्ञान को भी दूर नहीं किया है और उसके परिणाम-अहंकार (अहंभाव) और देह में आत्मा का अध्यास भी अभी निवृत्त नहीं हुए। मृत्यूपरान्त, अगले जन्म में भी अशुभ संस्कारों के पर वश हुआ वह अशुभ कर्म में पुनः प्रवृत्त हो जाता है। किन्तु आत्म ज्ञानी समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है क्यों कि पापों का मूल कारण अज्ञान और उसके परिणाम, देह को ही आत्मा मान लेना, पूर्ण रूपेण पापों और संस्कारों सहित नष्ट हो जाते हैं। भुने हुए बीजों की भाँति संस्कार पूर्ण रूप से भस्म हो जाते हैं। भस्म हुए बीज जैसे पुनः अंकुरित नहीं हो सकते वैसे ही दग्ध संस्कार पुनः कर्म और पुनर्जन्म नहीं दे सकते ।
अन्य (निम्नलिखित) कारण से भी मैं लोकों का शासक हूँ।
बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ।।४ ।।
शब्दार्थ : बुद्धि बुद्धि, ज्ञानम् - ज्ञान, असंमोहः - असंमोह (ज्ञान), क्षमा-क्षमा, सत्यम् -सत्य, दमः- आत्म संयम, शमः-शान्ति, सुखम् -सुख, दुःखम् दुःखा, भव-अस्तित्व, अभाव:-अभाव (अनस्तित्व), भवम् -भय,च- और, अभयम्-अभय, एव -ही, च -और ।
अनुवाद : निश्चयात्मिका बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढता, क्षमा, सत्य, मनोनिग्रह, इन्द्रिय-निग्रह, सुख-दुःख, अस्तित्व (जन्म), अनस्तित्व (मृत्यु), भय और अभय भी
व्याख्या: अन्तःकरण चतुष्टय-मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में बुद्धि सूक्ष्म विषयों को समझने की एक शक्ति है। आत्म ज्ञान ही ज्ञान अथवा बुदि है। भ्रमरहित होना असंमोह है। किसी भी क्षण कोई कार्य सम्पन्नता अथवा ज्ञान प्राप्ति के समय विवेक से काम लेना ही असंमोह है। अपमान होने पर मन की अनुद्विग्नता धैर्य है। आक्रमण करने वाले अथवा अपशब्द बोलने वाले के प्रति बुरा भाव न रखना भी धैर्य है । तीनों प्रकार के ताप-आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, बिना रुदन किये सहन करना धैर्य है। ज्वर आदि आध्यात्मिक ताप हैं। अति शीत, अत्युष्णता, अति वृष्टि, मेघ गर्जन और विद्युतपात आदि आदिदैविक ताप है। वन्य-पशुओं से भय, वृश्चिकदंश,सर्पदंश आदि अधिभौतिक ताप हैं।
सत्य, सत्यवादिता है। श्रुत (श्रवण किये गये) अथवा दृष्ट (देखे गये। विषयों के प्रति अपना वास्तविक अनुभव बताना सत्यवादिता है। इसमें किंचित् मात्र भी अतिशयोक्ति अथवा तथ्यों की अल्प मात्र भी परिणति नही होती। बाह्य इन्द्रियों का निग्रह दम है। यह कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका के अपने विषय-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध से इन्द्रियों का संहरण है। शम मन की शान्ति है जो इन्द्रिय-विषयों से मन को हटा कर और मनोनिग्रह से प्राप्त होती है।
सुखम् सुख, धर्म के अनुरूप जीवन जो समस्त प्राणियों के लिए भी अनुकूल है, सुख कहलाता है। दुःख का मुख्य कारण अधर्म है जो समस्त प्राणियों के लिए प्रतिकूल है, दुःखद है।
जो दिखाई देता है वह भाव है। सत् भाव है और असत् अथवा अवास्तविकता अभाव है।
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ।।५ ।।
शब्दार्थ : अहिंसा-अहिंसा, समता-सम भाव, तुष्टिः सन्तोष, तपः-तपस्या, दानम् -दान, यशः- यश, अयशः-अयश, भवन्ति-होते हैं, भावा:-भाव (गुण), भूतानाम् -प्राणियों के, मत्तः- मेरे से, एव-ही, प्रकार के।
अनुवाद : अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश-प्राणियों के ये विभिन्न प्रकार के गुण मुझ से ही उत्पन्न होते हैं।
व्याख्या: मनसा, वाचा, कर्मणा किसी प्राणी को चोट न पहुँचाना अहिंसा है। समता वह अवस्था है जिसमें मनुष्य प्रिय-अप्रिय को प्राप्त कर के राग और देष से मुक्त रहता है। इस मानसिक अवस्था में प्रिय अथवा अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति पर विषाद नहीं होता । तुष्टि सन्तोष है। सन्तुष्ट व्यक्ति प्रारब्ध से प्राप्त प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहता है। वह अपनी वर्तमान उपलब्धियों में प्रसन्न है । वह लोभ से मुक्त है अतः शान्त मन से विचरण करता है। सन्तोष मनुष्य को अत्यन्त धनवान बना देता है। यह लोभ को मारता है। लोभ तो धनवान को भी भिखारी बना देता है। लोभी मनुष्य सदा अशान्त रहता है। शनैः शनैः भोजन की मात्रा कम करने और उपवास के अभ्यास द्वारा शरीर और इन्द्रियों का संयम तपस् है। शरीर व इन्द्रियों की शक्ति उपवास द्वारा क्षीण होती है।
धनम्-यह उपकारपरता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी धन-सम्पत्ति का दान करना ही उपकार है। सुपात्र को शुभ देश काल में धान, स्वर्ण, वस्त्र आदि देना और विशेष कर ऐसे पात्र को देना जो प्रत्युपकार में आपके लिए कुछ न कर सकता हो, 'धनम्' का गुण है।
यशस् - धर्म अथवा सद्गुणों से ख्याति यश है।
अयशस् - अधर्म अथवा पाप कर्मों से अकीर्ति अयश है।
प्राणियों के कर्मानुसार ये विभिन्न प्रकार के गुण, समस्त लोकों के स्वामी, मुझ से उद्भूत हैं।
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।।६ ।।
शब्दार्थ : महर्षयः - महान् ऋषि, सप्त-सात, पूर्वे-सनातन, चत्वारः- चार, मनवः मनु, तथा-और, मद्भावाः- मेरी शक्तियों से युक्त (मुझ में भाव वाले), मानसाः-मन से, जाताः-उत्पन्न, येषाम् -जिनकी, लोके-संसार में, इमाः– ये, प्रजाः सन्तान, प्राणी।
अनुवाद : सात महर्षि, चार उनसे पूर्व होने वाले (सनकादि) और कर जो मेरी ही शक्तियों से युक्त है (क्योंकि उनके मन मेरे में एकाग्र है), वे सबसे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और संसार की समस्त प्रजा उनसे में मैं अकेला था, एक ही उत्पन्न है।
व्याख्या : प्रारम्भ में मैं अकेला था, और मुझसे मन हुआ और मन से सात ऋषि (भृगु, वसिष्ठ आदि), चार सनातनः सनन्दन, सनत्कुमार और सनत्सुजाता) और पूर्व काल के सावर्णि आदि चार मनु, इन सब ने अनन्य मन से मेरा ध्यान किया इसलिए ये सब दिव्य शक्तिये और उत्कृष्ट परम ज्ञान से युक्त हुए।
पावन चार युवा कुमारों ने परिणय सूत्र में बंध कर सन्तानोत्पत्ति करने के भाव को त्याग दिया। उन्होंने ब्रह्मचारी रह कर ब्रह्मविचार का अभ्यास अथवा ब्रह्म पर गहन ध्यान का संकल्प लिया।
वे सब मेरे द्वारा मेरे संकल्प से अस्तित्व में आये। वे सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सामान्य मनुष्य की भाँति वे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। चराचर जगत के समस्त प्राणी सप्तर्षियों और चार मनुओं की सन्तान हैं। महान ऋषि ब्रह्म विद्या अर्थात् उपनिषदों के शाश्वत ज्ञान के प्रथम आचार्य थे। मनु मनुष्णे के शासक थे। मानवता के उद्धार और पथ-प्रदर्शन हेतु उन्होंने आचार-संहिता और धर्म संहितायें बनाईं।
सात महान् ऋषि सात लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्माण्ड में महत् अथवा वैश्विक बुद्धि, अहंकार अथवा वैश्विक अहम् और पंचतन्मात्र अथवा पंच-मूल-तत्त्व जिनमें पाँच महान् तत्त्व पृथ्वी, जल, पावक, समीर और गगन स्थूल रूप हैं-सात ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चराचर स्थूल जगत् और सूक्ष्म आन्तरिक जगत् इन सात तत्त्वों से प्रकट हुए है। पुराणवृत्त में इन सात तत्त्वों को लक्षणा से सात मानवीय नामों से लक्षित किया गया है। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ-ये सात ऋषि हैं।
सूक्ष्म जगत् में मनस् (मन), बुद्धि, चित्त और अहंकार चार मनुओं को लक्षित करते हैं और उन्हें मानव-नाम दिये गये हैं। प्रथम समूह त्रिभुवन का आधार बनाता है। द्वितीय समूह सूक्ष्म जगत् (व्यष्टि जगत्) का आधार बनाता है। ये दो समूह वैज्ञानिक जीवन के इस विशाल ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं।
मद्भावा-मेरी प्रकृति से युक्त, मुझ में समाहित।
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ।।७।।
शब्दार्थ : एताम्-इस, विभूतिम् -विभूति को, योगम् - योग शक्ति को, और, मम- मेरी, य:- जो, वेत्ति -जानता है, तत्वतः तत्त्व से, स: -वह, अविकम्पेन -निश्चल, योगेन -योग से, युज्यते-युक्त हो जाता है, न -नहीं, अत्र-यहाँ (इसमें), संशयः- संशय।
अनुवाद : जो पुरुष मेरी इन विविध रूप अभिव्यक्तियों और योग शक्ति को तत्त्व से जानता है वह निश्चल योग में स्थित हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं।
व्याख्या : भगवान् की ऐश्वर्यमयी विभूति का ज्ञान वस्तुतः योग में हितकर है। भगवान् की अभिव्यक्तियों और विविध विभूतियों की कारण रूपा उनकी अन्तरस्थ सर्वव्यापी शक्ति को तत्त्व से जानने वाला व्यक्ति उनके साथ अटल योग से एकत्व प्राप्त कर के शाश्वत शान्ति और पूर्ण समत्व को प्राप्त होता है। चींटी से लेकर ब्रह्मापर्यन्त भगवान् के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। जो भगवान् की इस विस्तृत अभिव्यक्ति और योग को जानता है, वह दृढ़ अविकम्प योग से युक्त हो जाता है। (अभिव्यक्ति और योग में-योग का अभिप्राय है जो योग से प्रकट हुआ है अर्थात् अनन्त यौगिक शक्तियाँ और सर्वज्ञता)। वह नित्य सत्ता में वास करता है और आत्मा के सर्वोच्च, उत्कृष्ट ज्ञान से संपन्न होता है। इस सत्य का ज्ञान करने पर मनुष्य वरीयता (superiority) और हीनता (inferiority) के भावों से मुक्त हो जाता है। उसमें वास्तविक ज्ञान का उदय होता है। वह सब प्राणियों में भगवान् के और भगवान् में सब प्राणियों के दर्शन करता है। वह किसी जीव से घृणा नहीं करेगा। यह एक विरल वैश्विक अनुभूति है। योगी जान लेता है कि भगवान् तथा उनकी अभिव्यक्तियाँ पृथक् पृथक् नहीं हैं, एक ही हैं। वह परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है और अनन्य भक्ति भाव से उसमें (भगवान् में) समा जाता है। मेरे दिव्य योग के द्वारा उसे परमात्मा के साथ एकत्व की पूर्ण जागृति होती है।
परमात्मा के साथ अपने एकत्व की चेतना को बिना खोये वह किया भी परिस्थिति और परिवेश में अपने मन का सन्तुलन बनाये रखने में सक्षम होगा है। (निरूपण-VII.25; IX.5; X1.8)
वह अविचल योग कौन सा है जिससे वे युक्त होते हैं? उत्तर है...
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।।८ ।।
शब्दार्थ : अहम् -मैं, सर्वस्य -सब का, प्रभवः- स्रोत, मत्तः -मुझसे, सर्वम् -सर्वस्व, प्रवर्तते-उत्पन्न होता है, इति-इस प्रकार, मत्वा-समझ कर, भजन्ते -आराधना करते हैं, , माम् -मेरी, बुधाः- ज्ञानीजन,भावसमन्विताः- ध्वान युक्त होकर ।
अनुवाद : मैं सब का मूल स्रोत हूँ। मुझ से सर्व सृष्टि के पदार्थ अस्तित्व में आते हैं। इस प्रकार समझकर बुद्धिमान् लोग भावपूर्ण हृदय से मेरा ही भजन करते हैं।
व्याख्या : जल में लहरें उठती हैं उसी पर आधारित रहती हैं और अन्त में जल में ही लीन हो जाती हैं। लहरों का एकमात्र अवलम्बन जल है। इसी भाँति सम्पूर्ण जगत् का एकमात्र अवलम्बन भगवान् है। इतना विवेक होने बर विद्वान् भगवान् की सर्वात्मकता का अनुभव करते हुए भक्ति और प्रेम से उसकी आराधना करते हैं। सब देशों में, सब कालों में परम पुरुष तो वही एक । वह निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है।
अव्यक्त मूल प्रकृति के रूप में भगवान् सब रूपों का स्रोत है। वे अव्युत्पन्न जगत् हैं। वे अपनी शक्ति (क्रियात्मक शक्ति) पर दृष्टिपात करते हैं और सम्पूर्ण जगत् का उद्भव होता है और रूप गतिशील होते हैं। कुशाग्र और क्ष्म बुद्धि से शून्य सांसारिक व्यक्ति परिवर्तशील स्वरूपों को स्थूल नेत्रों से देखता है। भीतर विराजित आत्मा, अवलम्बन, सर्वव्याप्त बुद्धि अथवा आनन्द स्वरूप चेतना का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वह तो अनित्य रूपों में आकृष्ट होता है। इन क्षणिक रूपों में वह अपने सुख और आशाओं को ढूँढता है। उन्हीं के लिए वह जीता है और संघर्ष करता है। पत्नी और सन्तान की प्राप्ति पर वह ल्लास में झूमता है ये रूप यदि लुप्त हो जायें तो दुःख के सागर में डूब जाता है। किन्तु बुद्धिमान् सदा परमात्मा में वास करते हैं जो सब जीवों का प्रभव है। वे उस सच्चिदानन्द स्वरूप अमर अन्तरात्मा में, जो उनका अपना ही अद्वैत आत्मा है, आनन्द लेते हैं, यद्यपि उनके सर्वतः रूप परिवर्तित होते रहें अथवा लुप्त होते रहें उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे योग में दृढ़ हैं। वे अचल योग से युक्त हैं। वे योग में अभिषिक्त हैं अर्थात् योग रूपी सिंहासन पर आरूढ़ हैं। गहन ध्यान में वे परमात्मा की वन्दना करते हैं और अनिर्वचनीय निर्विकल्प समाधि का आनन्द लेते हैं।
वासुदेव के रूप में परब्रह्म समस्त संसार के मूल कारण हैं। उन्हीं से सृष्टि का उद्भव और विकास समस्त परिवर्तनों सहित अर्थात् स्थिति, विनाश, क्रिया, फल और भोग होता है। इतना जान कर ज्ञानी परम पुरुष की आराधना करते हैं और परमात्मा में समाधिस्थ होते हैं। (निरूपण - IX.10)
मच्चित्ता मगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ।।९ ।।
शब्दार्थ : मच्चित्ताः मुझ में पूर्णतया चित्त लगाने वाले, मद्रतप्राणा:-मुझ में ही, प्राणों को अर्पित करने वाले, बोधयन्तः- बोध करते हुए, परस्परम् - आपस में, कथयन्तः-कहते हुए, च-और, माम् -मुझे, नित्यम् -नित्य, तुष्यन्ति-संतुष्ट होते हैं, च-और, रमन्ति-प्रसन्न होते हैं, च और ।
अनुवाद : अपने मन और जीवन मुझ में लीन कर के एक-दूसरे को ज्ञान-प्रकाश देते हुए और सदा मेरा गुणगान करते हुए वे प्रसन्न और सन्तुष्ट रहते हैं।
व्याख्या : ईश्वर सायुज्य प्राप्त करने वाले भक्तों की विशेषताओं का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। भक्त सतत भगवद् चिन्तन करता है। उसका जीवन ही उसी को समर्पित होता है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार-उसकी समस्त इन्द्रियाँ (जो प्राण के कारण गतिशील होती हैं) जैसे नेत्र आदि सब भगवान् में लीन हो जाती हैं। भगवत्चर्चा में उसे अपार हर्ष होता है। उनके अलौकिक बुद्धिसामर्थ्य, विलक्षण शक्ति, पराक्रम एवम् अन्य विभूतियों का वह गुणगान करता है। वह पूर्णतया भगवान् को समर्पित होता है। वह इतने आनन्द और तुष्टि का अनुभव करता है मानो अपने प्रियतम (भगवान्) की सन्निधि में हो। पुराण का कथन है-भूलोक के समस्त विषय-सुख और स्वर्गलोक के अनन्त सुख मिला कर उस आनन्द का सोलहवाँ अंश भी नहीं है जो इच्छाओं और तृष्णाओं को मिटाने से प्राप्त होता है। (निरूपण-XII.8)
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।।१० ।।
शब्दार्थ : तेषाम् - उनको, सततयुक्तानाम् -नित्य युक्त, भजताम् -पूजा करते हुए, प्रीतिपूर्वकम् -प्रेमभाव से, ददामि देता हूँ, बुद्धियोगम् - विवेकयोग, तम्-उस, येन-जिसके द्वारा, माम् -मुझे, उपयान्ति-प्राप्त होते हैं, ते-वे।
अनुवाद : योग में नित्य युक्त प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाले (साधकों) को मैं विवेकयोग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त होते हैं।
व्याख्या : वही भक्त दिव्य (दैवी) कृपा के अधिकारी होते हैं जो भगवान् को समर्पित हैं, सदा समन्वित (समरस) हैं, आत्मस्थ हैं, भक्तियुक्त हैं और अनन्य प्रेम से उसकी आराधना करते हैं, स्वार्थभाव से नहीं। भगवान् उन्हें आत्म-ज्ञान की प्राप्ति हेतु बुद्धियोग प्रदान करते हैं। उन पर चित्त निमग्न करने वाले भक्तों को भगवान् सम्यक् ज्ञान की भक्ति (बुद्धियोग) प्रदान करते हैं जिससे भक्तगण उन्हें तत्त्व से जान सकें। गहन ध्यान में प्रज्ञा चक्षु के द्वारा वे उस परमात्मा के दर्शन करते हैं जो सब में एक है, सब का आत्मा है और सब सीमाओं से परे है, उसे वे निज आत्मा के रूप में देखते हैं। यहाँ 'बुद्धि' शब्द अन्तर्ज्ञान के नेत्र का संकेत करता है जिसके द्वारा एकत्व का विलक्षण, अलौकिक अनुभव प्राप्त होता है। बुद्धियोग ही ज्ञान योग है। (निरूपण -IV.39.XII.6.7)
भगवान् अपने भक्तों को यह बुद्धि योग क्यों देते हैं? साधक अथवा भक्त के मार्ग की कौन सी कठिनाइयों को बुद्धि योग दूर करता है ? इसका उत्तर अगले श्लोक में है।
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।।११।।
शब्दार्थ : तेषाम् -उनके, एव-ही, अनुकम्पार्थम् - अनुग्रह करने के लिए , अहम् -मैं, अज्ञानजम्-अज्ञान से उत्पन्न, तमः - अन्धकार, नाशयामि -नाश करता हूँ, आत्मभावस्थ:- आत्मा में स्थित, ज्ञानदीपेन-ज्ञान दीप के द्वार, भास्वता- प्रकाशमान् ।
अनुवाद : उनके अन्तःकरण में विराजित मैं केवल उन पर अनुकम्पा कर के उनके अज्ञान जनित अन्धकार को ज्योतिर्मय ज्ञान के दीप से दूर करता है।
व्याख्या : ज्ञान दीपेन भास्वता-भगवान् उन भक्तों के हृदय में सतत भास करते हैं जो अनवरत रूप से उनका चिन्तन करते हैं। वे उनके भीतर के अविवेक से उत्पन्न अज्ञानान्धकार के आवरण को ज्ञान के ऐसे प्रकाशमान् दीप हे दूर करते हैं जिसमें पवित्र भक्ति का तेल हो, गहन ध्यान की स्वच्छ निर्मल वायु का उद्दीपन (पंखा) हो, सतत ब्रह्मचर्य के अभ्यास, शुचिता तथा अन्य दिव्य गुणों से उद्भूत सहजावबोध की वर्तिका (बाती) हो, जिसका आलंबन सांसारिकता से शून्य हृदय कोष्ठ हो, स्थिति मन के अन्तस्तम कोण में हो जो विषय-वासनाओं के झोंके (हवा) से दूर हो, राग-द्वेष से रहित निष्कलंक हो और ध्यान के अनवरत अभ्यास के कारण प्राप्त ज्ञान के प्रकाश से देदीप्यमान हो ।
दीप को अन्धकार हटाने के लिए किसी साधन अथवा किसी प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अन्धकार के निवारण हेतु मात्र प्रकाश उत्पन्न करना ही पर्याप्त है। प्रकाश के द्वारा अन्धकार दूर होता है, पात्र, कुर्सी आदि सभी-वस्तुएँ दृष्टिगत होने लगती हैं। एवंविध आत्म-ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान स्वयं दूर होने लगता है। किसी अन्य कर्म अथवा अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। आत्म-ज्ञान का सूर्य जब अज्ञान रूप अन्धकार को दूर करता है तो केवल ब्रह्म ही अपनी अपूर्व महिमा से अभिभासित होता है।
अर्जुन उवाच
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ।।१२ ।।
शब्दार्थ : परम् -परम, ब्रह्म-ब्रह्म, परम् - परम, धाम-धाम (आश्रय), पवित्रम् - पवित्र, परमम् -परम, भवान् -आप, पुरुषम् -पुरुष, शाश्वतम्- शाश्वत, दिव्यम् - दिव्य, आदिदेवम् -सनातन देव, अजम् - जन्मरहित, विभुम् - सर्वव्यापक ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : आप परम ब्रह्म है, परम धाम है (परम प्रकाश स्वरूप है) परम पवित्र हैं, शाश्वत हैं, दिव्य पुरुष है, सनातन देव है, जन्मरहित और सर्वव्यापक हैं।
"व्याख्या : परं ब्रह्म-सर्वोच्च आत्मा । परं शब्द पावन निर्गुण नित्य तत्व (परमात्मा) की ओर संकेत करता है जो सीमित अनुबंधों से परे हैं। यह सच्चिदानन्द ब्रह्म है। गौण ब्रह्म सगुण ब्रह्म (ईश्वर) है अथवा सीमित अनुबंधों सहित ब्रह्म है अथवा भक्तों द्वारा चयन किया गया ध्यान का विषय है जिसे ब्रह्म की संज्ञा दी जाती है।
परम धाम-परम तेजः । ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त परब्रह्म ही सब का आधार है इसीलिए उसे परम धाम (आश्रय स्थल) कहा जाता है।
आदि देव-सनातन शाश्वत ब्रह्म जो सब देवों से पूर्व भी अस्तित्ववान् था। यह परं ब्रह्म है और स्वयं प्रकाश है।
पवित्रं परमम्-परम पवित्रकर्त्ता । पावन नदियाँ और धार्मिक वीर्थस्थल केवल पापों का विनाश कर सकते हैं किन्तु परं ब्रह्म समस्त पापों को नके मूल कारण, अज्ञान को भी नष्ट करने में सक्षम है। अतः परम नित्य तत्त्व को परम पवित्र कहा गया है।
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ।।१३ ।।
शब्दार्थ : आहुः-कहते हैं, त्वाम् - आपको, ऋषयः -ऋषिगण, सर्वे-सब, देवर्षि-देवर्षि, नारदः - नारद, तथा-भी, असितः -असित, देवल:-देवल, व्यासः - व्यास, स्वयम्-आप, च-और, एव-ही, प्रवीषि-कहते हो, मे-मुझे।
अनुवाद : समस्त ऋषि, देवर्षि नारद भी और असति, देवल, व्यास ने आपके लिए (ऐसी) घोषणा की है और अब आप मुझे भी वही कह रहे हैं।
व्याख्या: ऋषि-संयत मन और इन्द्रियों से युक्त पवित्र तपस्वी ऋषि देवर्षि-ऋषि से भी उत्कृष्टतर, दैवी ऋषि ।
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ।।१४।।
शब्दार्थ : सर्वम् -सब, एतत्-यह, ऋतम् -सत्य, मन्ये-मानता हूँ, यत्-जो, माम् -मुझे, वदसि—आप कहते हैं, केशव- हे केशव, न-नहीं, हि-निश्चित रूप से, ते -आपका, भगवन् - हे भगवन्, व्यक्तिम् - अभिव्यक्ति, विदु-जानते हैं, देवा- देवगण, न-नहीं, दानवाः-असुर ।
अनुवाद : हे केशव, आप मुझे जो कुछ भी बता रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। निश्चित रूप से भगवन्, न तो देवता और न ही दानव आपके उद्भव (अभिव्यक्ति) को जानते हैं।
व्याख्या : भगवान् वह है जिसमें छः गुण पूर्णता में विद्यमान हों। वे गुण हैं-ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, श्री और बल। और भी जो समस्त प्राणियों के उद्भव, प्रलय और भविष्य को जानता है और जो सर्वज्ञ है वह भगवान् है।
व्यक्ति-उद्भव ।
दानवः राक्षस ।
अर्जुन भगवान् को केशव (सब का स्वामी) कह कर पुकारते हैं क्योंकि भगवान् जानते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। क्योंकि भगवान् ही देवों और दानवों तथा अन्य प्राणियों के मूल स्रोत हैं। अतः वे भगवान् की अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं कर सकते।
स्वयमेवात्मनाऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ।।१५ ।।
शब्दार्थ : स्वयम् - आप स्वयं, एव-ही, आत्मना-आत्मा से, आत्मानम् - आत्मा को, वेत्थ-जानते हो, त्वम्-आप, पुरुषोत्तम- हे पुरुषोत्तम, भूतभावन-प्राणियों के स्रोत, भूतेश-जीवों के स्वामी, देवदेव-देवों के देव, जगत्पते-जगत् के स्वामी।
अनुवाद : हे पुरुषोत्तम, हे जीवों को उत्पन्न करने वाले, उन पर शासन करने वाले भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत् नियन्ता प्रभु आप स्वयं ही अपनी आत्मा से आत्मा को जानते हो अर्थात् अपने द्वारा स्वयं को जानते हो ।
व्याख्या: पुरुषोत्तम का अभिप्राय है पुरुषों में उत्तम (सर्वश्रेष्ठ)। ये चार रूप धारण करते हैं-भूतभावन, भूतेश, देवदेव और जगत्पति, अत: वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं।
देवदेव-इन्द्र और अन्य देवता भी जिसकी पूजा करते हैं वे देवदेव है।
जगत्पति-भगवान् संसार की रक्षा करते हैं और वेदविहित आदेशों के अनुरूप संसार का पथ-प्रदर्शन करते हैं अतः वे जगत्पति हैं।
वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ।।१६ ।।
शब्दार्थ : वक्तुम् -कहने में, अर्हसि -समर्थ हैं, अशेषेण-पूर्णता से, दिव्या-दिव्य, हि-निश्चित रूप से, आत्मविभूतयः अपनी विभूतियों को, याभिः- जिनके द्वारा, विभूतिभिः - विभूतियों से, लोकान् -लोकों को, इमान् -इन, त्वम् -आप, व्याप्य-व्याप्त करके, तिष्ठसि-स्थित हैं।
अनुवाद : जिन विभूतियों से इन लोकों में व्याप्त हो कर आप स्थित हैं उन दिव्य विभूतियों का पूर्ण रूप से वर्णन करने में निश्चयेन आप ही समर्थ हैं।
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।।१७ ।।
शब्दार्थ : कथम् कैसे, विद्याम् - जानूँ, अहम् - मैं, योगिन् -हे योगेश्वर, त्वाम् आपको, सदा-सदा, परिचिन्तयन् - ध्यान करता हुआ, केषु-केषु -किन-किन, च-और, भावेषु-भावों में, चिन्त्यः - चिन्तन के योग्य, असि-हो, भगवन् -हे भगवन्, मया-मेरे द्वारा।
अनुवाद : हे योगेश्वर, किस प्रकार आपका ध्यान करता हुआ मैं आपको जान सकूँगा? हे भगवन्, आप किन-किन भावों में मेरे द्वारा चिन्तन के योग्य हैं?
व्याख्या : अर्जुन ने कहा- "हे भगवन्, सतत ध्यान द्वारा मैं आपको किस प्रकार जान सकता हूँ? किन भावों में आप मेरे चिन्तन में आ सकते हैं? यदि मुझे आपकी विभूतियों का ज्ञान हो तो बाह्य विषयों की विशेष अभिव्यक्तियों में भी मैं आप पर अपना मन स्थिर कर सकता हूँ। अतः मुझ पर अनुज्ञा कर के अपनी विभूतियों का निःशेष रूप से वर्णन कीजिए। तभी मैं सर्वत्र समस्वरूप (एकत्व) दर्शन कर सकने में सक्षम हो सकता हूँ।
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।
भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ।।१८ ।।
शब्दार्थ : विस्तरेण -विस्तार से, आत्मनः अपना, योगम् -योग, विभूतिम् - विभूति को, तुष्टि, और, जनार्दन से जनार्दन, भूय:-पुन:, कथय- कहो, तृप्तिः सन्तुष्टि, हि-क्योंकि, शृण्वतः सुनते हुए, न नहीं, अस्ति-है, मे -मेरी, अमृतम् अमृत ।
अनुवाद : हे कृष्ण, अपनी विभूति और योग शक्ति का पुनः विस्तार से वर्णन कीजिए क्योंकि आपकी प्राण संचारिणी अमृतमयी वाणी का श्रवण कर के अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ।
व्याख्या : भगवान् को जनार्दन कहा जाता है क्योंकि सभी जनगण सफलता, सुख-समृद्धि और मोक्ष-प्राप्ति के लिए उनको ही प्रार्थना करते हैं। अर्जुन भी उनसे प्रार्थना कर रहा है कि भगवान् उसे अपनी योग शक्ति से परिचित करायें, विभूति के दर्शन करायें और उसे मोक्ष प्रदान करें।
अर्जुन भगवान् कृष्ण से कहते हैं- "विस्तार से मुझे अपनी रहस्यात्मक योग शक्ति और ऐश्वर्य के दर्शन कराओ और चिन्तनशील विषयों का उपदेश करो। यद्यपि सप्तम् और नवम् अध्याय में आपने समासतः (संक्षेप में) वर्णन किया है तथापि पुनः विस्तार से बताने की कृपा करें क्योंकि आपकी अमृतमयी वाणी सुन कर अभी तृप्ति नहीं हुई है। जितना अधिक श्रवण करता हूँ उतनी ही अधिक श्रवण की इच्छा बढ़ती है और मुझे सन्तुष्टि नहीं होती। निस्सन्देह यह मेरे लिए अनश्वरता का अमृत है।
श्री भगवानुवाच
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।।१९ ।।
शब्दार्थ : हन्त-अच्छा, अब, ते-तुम्हारे लिए, कथयिष्यामि -कहूँगा दिव्याः -दिव्य, हि -निश्चित रूप से, आत्मविभूतयः-अपनी विभूतियाँ, प्राधान्यतः - प्रधान रूप से, कुरुश्रेष्ठ- हे कौरवों में श्रेष्ठ, 7 - 76 , अस्ति-है. अन्त-अन्त, विस्तरस्य-विस्तार का, मे-मेरे।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : बहुत अच्छा (सुष्ठु), अब मैं अपनी दिव्य (देव लोक की) विभूतियों का प्रधान रूप से उपदेश करूँगा क्योंकि हे अर्जुन, उनके विस्तारपूर्वक वर्णन का तो कोई अन्त ही नहीं है।
व्याख्या : अब मैं तुम्हें अपनी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विभूतियों के विषय में बताऊँगा। मेरी महिमा अपरम्पार है, उन सब का वर्णन करना सम्भव नहीं है।
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ।। २० ।।
शब्दार्थ : अहम् मैं, आत्मा-आत्मा, गुडाकेश गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितः -सब प्राणियों के हृदय में स्थित, अहम् -मैं, आदि:-आदि, च-और, मध्यम् -मध्य, च-और, भूतानाम् -सब प्राणियों का, अन्तः- अन्त, एव-ही, चऔर।
अनुवाद : हे गुडाकेश (अर्जुन), मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ।
व्याख्या : हे गुडाकेश, सब जीवों के हृदय में स्थित प्रत्यगात्मा मैं हूँ। मैं ही सृष्टि के जीवों का उद्भव, स्थिति और अन्त हूँ, मैं ही सब का जन्म, जीवन और मृत्यु हूँ। अन्तस्तम आत्म रूप में मेरा ध्यान करो।
गुडाकेश-निद्राजयी अथवा घने बालों वाला।
अभेदभावना से आत्मा पर चित्त एकाग्र करने वाला प्रथम श्रेणी का अधिकारी साधक है। जो भगवान् पर चित्त एकाग्र करने, ध्यान लगाने में असमर्थ है, वे निम्नवर्णित विषयों में भगवान् का ध्यान करें। मध्यम श्रेणी के साधकों के लिए यह ध्यान की विधि है।
आदित्यानामहं विष्णुर्थ्योतिषां रविरंशुमान् ।
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ।।२१ ।।
शब्दार्थ : आदित्यानाम् - आदित्यों में, अहम् -मैं, विष्णुः - विष्णु, ज्योतिषाम् - ज्योतियों में, रविः-सूर्य, अंशुमान्-देदीप्यमान (किरणों से युक्त), प्ररीचि मरीचि, मरुताम्मरुतों (वायु देवताओं) में, अस्मि हूँ, नक्षत्राणाम्-नक्षत्रों (सितारों) में, अहम् -मैं, शशी-चन्द्रमा।
अनुवाद : (बारह) आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं प्रकाशमान् सूर्य है, सप्त या उनचास मरुतों में मैं मरीचि हैं। नक्षत्रों में मैं चन्द्रमा है।
व्याख्या : द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु आदित्य हूँ। धत्त (Dhatta), चित्र, अर्थमा, रुद्र, वरुण, भग, सूर्य, विवस्वान, पूषन्, सविता, त्वष्टा और विष्णु वे द्वादश आदित्य हैं। वर्ष के द्वादश मास आदित्य हैं।
वायुओं को नियन्त्रित करने वाले देव मरुत हैं। कुछ लोग उनकी गणना झात मानते हैं, अन्य उन्चास मानते हैं।
द्वादश आदित्य, अग्नि, विद्युत आदि ज्योतियां, मरुत, नक्षत्र आदि भावान् की सामान्य विभूतियां हैं। विष्णु, सूर्य, मरीचि और चन्द्र विशेष विभूतियां हैं इसीलिए उनमें अपेक्षाकृत अधिक तेज है।
सूर्य और चन्द्रमा पर भगवान् को अधिष्ठित कर के उनको भगवान् के रूप मान कर उन पर ध्यान कर सकते हैं। इस अध्याय के आगे के श्लोकों में दिये गये रूपों पर भी आप ऐसे ही ध्यान कर सकते हैं।
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ।।२२ ।।
शब्दार्थ : वेदानाम् -वेदों में, सामवेदः-सामवेद, अस्मि (मैं) हूँ, देवानाम् देवों में, अस्मिㅡ (मैं) हूँ, वासवः- इन्द्र, इन्द्रियाणाम् - इन्द्रियों में, मनः-मन, च-और, अस्मिㅡ(मैं) हूँ, भूतानाम् - जीवों में, अस्मि (मैं) हूँ, चेतना-चेतना ।
अनुवाद : वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इन्द्र हूँ, इन्द्रियों में मन और जीवों में मैं चेतना हूँ।
व्याख्या : वासवः इन्द्र, देवा:-रुद्र, आदित्य आदि देवता ।
इन्द्रियाः-पाँच ज्ञानेन्द्रियां अर्थात् कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका (घ्राणेन्द्रिय) ।
पाँच कर्मेन्द्रियां-वाक्, हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ। मन को ग्यारहवीं इन्द्रिय माना जाता है। मन के बिना इन्द्रियां अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकतीं इसलिए मन प्रमुख इन्द्रिय है।
चेतना-बुद्धि की वह चैतन्यावस्था जो शरीर और इन्द्रियों में समग्रता से विद्यमान है अथवा व्याप्त है। बुद्धि से लेकर स्थूल पर्यन्त जो सब को प्रकाशित करती है वह चेतना है।
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ।।२३ ।।
शब्दार्थ : रुद्राणाम् - रुद्रों में, शंकरः-शंकर, च-और, अस्मि (मैं) हूँ, वित्तेश-कुबेर, यक्षरक्षसाम् यक्ष और राक्षसों में, वसूनाम् वसुओं मैं, पावकः पावक (अग्नि), च-और, अस्मिㅡ (मैं) हूँ, मेरु:- मेरु, शिखरिणाम् - पर्वतों में, अहम् मैं।
अनुवाद : रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। वसुओं में मैं पावक (अग्नि) हूँ और सात पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ।
व्याख्या : रुद्र ग्यारह (एकादश) हैं, दस प्राण वायु (पाँच मुख्य प्राण और पंच उप प्राण) और मन । इन्हें रुद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर त्याग के समय ये दुःख देते हैं (रुलाते हैं)। पुराणों में ये इस प्रकार लक्षित किये गये हैं-वीरभद्र, शंकर, गिरीश, अजाइकपटी (Ajaikapti), भुवनाधीश्वर, अहर्भुज्य, पिनाकी, अपराजिता, कपाली, स्थाणु और भग। इन रुद्रों में शंकर प्रमुख हैं।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं। इन्हीं से समस्त ब्रह्माण्ड अवधृत है इसीलिए ये वसु हैं। पुराणों में इन्हें आपः, ध्रुव, सोम, धरा, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास नामों से आलक्षित किया गया है। इनमें अनल अथवा पावक (अग्नि) प्रमुख वसु हैं।
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ।।२४ ।।
शब्दार्थ : पुरोधसाम् -पुरोहितों में, च-और, मुख्यम् -प्रमुख, माम् -मुझे, विद्धि-जानो, पार्थ- हे पार्थ, बृहस्पतिम् - बृहस्पति, सेनानीनाम् - सेनापतियों में, अहम् -मैं, स्कन्दः स्कन्द, सरसाम्-जलाशयों में, अस्मि (मैं) हूँ, सागर:- समुद्र ।
अनुवाद : (राजाओं के) गृहस्थ पुरोहितों में हे अर्जुन, मैं बृहस्पति हूँ। सेनापतियों में मैं स्कन्द हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ।
व्याख्या: बृहस्पति देवताओं के मुख्य पुरोहित हैं। वे इन्द्र के कुल सिकन्द-कार्तिकेय अथवा सुब्रह्मण्य हैं। वे देव सेना के सेनापति हैं। पुरोहित हैं।
जलराशि-चाहे प्राकृतिक जलाशय, झील आदि ही हों मैं उनमें सागर हूँ।
महषींणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ।।२५ ।।
शब्दार्थ : महर्षीणाम् -महर्षियों में, भृगुः- भृगु, अहम् -मैं, विद्याम् शब्दों में, अस्मि (मैं) हूँ, एकम् - एक, अक्षरम् अक्षर, यज्ञानाम् यज्ञों में, जपयज्ञः जपयज्ञ, अस्मि (मैं) हूँ, स्थावराणाम् - स्थिर रहने बालों में, हिमालयः - हिमालय ।
अनुवाद : महर्षियों में मैं भृगु हूं। शब्दों में मैं एकाक्षर ॐ हूँ। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ।
व्याख्या : मनु ने कहा है-"ब्राह्मण कुछ और करे अथवा न करे, वह केवल जप से ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।"
भृगु-ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं।
हिमालय-विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला।
जपयज्ञ-इस यज्ञ में न तो कोई हिंसा है और न कोई हानि । इसीलिए समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ है।
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ।।२६ ।।
शब्दार्थ : अश्वत्थः- अश्वत्थ (पीपल), सर्ववृक्षाणाम् -सब वृक्षों में, देवर्षीणाम् देवर्षियों में, च-और, नारदः नारद, गन्धर्वाणाम् गन्धवौँ में, चित्ररथः-चित्ररथ, सिद्धानाम् -सिद्धों में, कपिलः-कपिल, मुनिः मुनि ।
अनुवाद : समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गन्धर्वी में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धों में कपिल मुनि हूँ।
व्याख्या : देवर्षि-देवता भी हैं और मन्त्र द्रष्टा ऋषि भी हैं।
सिद्धाः - बिना किसी प्रयास के जन्म के समय से ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने वाले सिद्ध कहलाते हैं।
मुनि-मनन अथवा आत्म-विश्लेषण और ध्यान करने वाले मुरि कहलाते हैं।
उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ।।२७ ।।
शब्दार्थ : उच्चैःश्रवसम् -उच्चैःश्रवस्, अश्वानाम् - अश्वों में, विद्धि- जानो, माम् -मुझे, अमृतोद्भवम् अमृत से उत्पन्न, ऐरावतम् -ऐरावत, गजेन्द्राणाम् -बड़े-बड़े हाथियों में, नराणाम् -मनुष्यों में, नराधिपम् -राजा । च-और,
अनुवाद : अश्वों में अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा मुझे जानो । श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत और नरों में नृप मुझे जानो।
व्याख्या : पयोधि को मथने पर अमृत की प्राप्ति हुई थी। उच्चैः श्रवा उस श्रेष्ठ अश्व का नाम है जो समुद्र-मन्थन के समय प्राप्त हुआ था।
ऐरावतम्-इरावती की सन्तान । इन्द्र का हाथी जो समुद्र-मन्थन के समय उत्पन्न हुआ था।
आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ।
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ।।२८ ।।
शब्दार्थ : आयुधानाम् - शस्त्रों में, अहम् - मैं, वज्रम् वद्भ, धेनूनाम् गौओं में, अस्मिㅡ(मैं) हूँ, कामधुक् -कामधेनु स्वर्गिक गाय जो सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, प्रजनः - उत्पत्ति का हेतु, च-और, अस्मि (मैं) हूँ, कन्दर्पः-कामदेव, सर्पाणाम् -सर्पों में, अस्मि-हूँ, वासुकिः - वासुकि ।
अनुवाद : शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। गौओं में इच्छित फल प्रदान करने वाली कामधेनु मैं हूँ। सन्तानोत्पत्ति का हेतु काम का देवता कामदेव मैं हूँ। सर्पों में मैं सर्पराज वासुकि हूँ।
व्याख्या : वज्र-दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना हथियार। युद्ध का एक साधन, जो केवल इन्द्र ही प्रयोग कर सकते हैं जिन्होंने सौ यज्ञ पूर्ण किये। कामधुक् - महर्षि वसिष्ठ की गाय जो समुद्र-मन्थन के समय उत्पन्न हुई और इच्छित फल प्रदान करने वाली है।
कन्दर्प-कामदेव ।
वासुकि:- सामान्य सर्पों का राजा । सर्प का केवल एक सिर होता है। बासुकि पीत वर्ण होता है। नागों के अनेक सिर होते हैं। अनन्तनाग अग्नि वर्ण का होता है।
श्रीधर के अनुसार सर्प विषैला होता है और नाग विषरहित होता है। रामानुज के अनुसार सर्प के एक ही सिर होता है और नाग के अनेक सिर होते हैं।
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ।।२९ ।।
शब्दार्थ : अनन्तः -अनन्त, च-और, अस्मि-हूँ, नागानाम् -नागों में, वरुणः - वरुण, यादसाम् -जल के देवताओं में, अहम् -मैं, पितृणाम् -पितरों में (पूर्वजों में), अर्यमा अर्यमा, च-और, अस्मि-मैं, यमः- यम, संयमताम् - शासन करने वालों में, अहम् - मैं।
अनुवाद : नागों में मैं अनन्तनाग हूँ, जल के देवताओं में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और शासन करने वालों में यम मैं हूँ।
व्याख्या : फणधारी सर्पों का राजा अनन्त है, इसे कोबरा भी कहते हैं और इसका अग्नि जैसा रक्त वर्ण है।
वरुण-जल के देवों का राजा।
यादसा:-जल से सम्बद्ध देवगण ।
अर्यमा पितरों का राजा ।
मैं यम हूँ, जीवों के समस्त कर्मों का साक्षी। सब के शुभाशुभ कर्मों का विगणन करने वाला।
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ।।३० ।।
शब्दार्थ : प्रह्लादः - प्रह्लाद, च-और, अस्मिㅡ (मैं) हूँ, दैत्यानाम् -दैत्यों में, कालः समय, कलयताम् - (काल) गणना करने वालों में, अहम् मैं, मृगाणाम् -पशुओं में, चऔर, मृगेन्द्र सिंह, अहम् -मैं, वैनतेय-विनत पुत्र गरुड़, च-और, पक्षिणाम् -पक्षियों में।
अनुवाद : दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूँ, गणकों में समय हूँ, पशुओं में मृगराज सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ।
व्याख्या : हिरण्यकश्यप दैत्य का पुत्र होते हुए भी प्रह्लाद भगवान् का भक्त था।
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ।।३१ ।।
शब्दार्थ : पवनः- पवन, पवताम् -पवित्र करने वालों में, अस्मि है, रामः -राम, शस्त्रभृताम् -शस्त्रधारियों में (योद्धाओं में), अहम् -मैं, झषाणाम् मछलियों में, मकरः मकर (शार्क), च-और, अस्मि-हूँ, स्रोतसाम् - नदियों में, अस्मि-हूँ, जाह्नवी-गंगा।
अनुवाद : पवित्र करने वालों में अथवा वेगवानों में मैं वायु हूँ, योद्धाओं में राम हूँ, मछलियों में मकर हूँ और नदियों में गंगा हूँ।
व्याख्या : स्वर्ग से भागीरथ जब गंगा को धरा पर ला रहे थे जाह्णू ने उसे निगल लिया इसलिए इसका नाम जाह्नवी पड़ा।
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ।। ३२ ।।
शब्दार्थ : सर्गाणाम् -सृष्टियों का, आदि: -आदि, अन्तः- अन्त, च-और, मध्यम् -मध्य, च-और, एव-भी, अहम् -मैं, अर्जुन-हे अर्जुन, अध्यात्मविद्या-आत्मा का ज्ञान, विद्यानाम् - विद्याओं में (विज्ञानों में), वादः-तर्क, प्रवदताम् - तार्किकों में, अहम् -मैं।
अनुवाद : सृष्टियों में मैं आदि, मध्य और अन्त हूँ। हे अर्जुन, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और वाद-विवाद करने वालों का बाद मैं हूँ।
व्याख्या : समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। ज्ञान की समस्त शाखाओं में मैं आत्म-ज्ञान हूँ। तार्किकों का मैं तर्क हूँ। वाद-विवाद करने वालों का मैं बाद हूँ। वाक्-विशारदों (प्रवक्ताओं) की मैं वाणी हूँ।
ऊपर श्लोक २० में भगवान् कहते हैं-
"मैं समस्त चराचर जगत् का आदि, मध्य और अन्त हूँ", यहाँ सम्पूर्ण सृष्टि का अर्थ सामान्य भाव में है।
आत्म-ज्ञान जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कराता है इसलिए ज्ञान की सब शाखाओं में यह प्रमुख है।
प्रवदताम् - विभिन्न प्रकार के लोग भिन्न-भिन्न रूप से अपना न्याय (तर्क) प्रस्तुत करते हैं जैसे—वाद, जल्प और वितण्डा वाद तर्क करने की वह विधि है जिससे किसी प्रश्न विशेष के मूल सत्य पर पहुँच सकते हैं। राग-द्वेष और ईष्यों से मुक्त साधकरण आपस में प्रश्नोत्तर करते हैं और सत्य की प्रकोष की समझने और सुनिश्चित करने हेतु दार्शनिक समस्याओं के वाद-विवकृत्ति देश करते हैं। एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए वे तर्क नहीं करते। यही बाद है। जल्प एक प्रकार का विसंवाद (झगड़ा) है जिसमें व्यक्ति अपने। यही को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने विपक्षी की बात का निराकरण (खंडन) करता है। वितण्डा, प्रतिपक्षी के तर्क में व्यर्थ का छिद्रान्वेषण करना है। प्रतिपक्षी के प्रश्नों को सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। जल्प और बितण्डा में साधक दूसरे को पराजित करने का प्रयास करता है। इसमें विजय की इच्छा निहित रहती है।
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ।।३३ ।।
शब्दार्थ : अक्षराणाम् - अक्षरों में, अकार:-अ (अकार), अस्मि (मैं) हूँ, द्वन्द्वः द्वन्द्व, सामासिकस्य-सब समासों में, च-और, अहम् -मैं, एव-निश्चित रूप से, अक्षयः- अक्षय (कभी क्षीण न होने वाला), कालः-समय, धाता-पोषण करने वाला, अहम् - मैं, विश्वतोमुखः सब ओर मुख वाला ।
अनुवाद : (वर्णमाला के) अक्षरों में मैं अकार हूँ, समासों में, द्वन्द्व समास हूँ। मैं निश्चित रूप से अक्षय (शाश्वत) काल हूँ। सब ओर मुख वाला मैं ही सब का धारण-पोषण करने वाला प्रणेता (कर्मफल प्रदाता) हूँ।
व्याख्या : वर्णों में मैं अकार हूँ। समासों में संयोगकारी द्वन्द्व समास मैं हूँ (समासों का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता होता है)। । काल का अर्थ यहां समय के आत्यन्तिक तत्त्व क्षण, मुहूर्त अथवा पल से है। काल परमेश्वर के लिए भी प्रयुक्त होता है क्योंकि वह काल का भी महाकाल है, कालातीत है।
क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है इसलिए कहा जाता है कि वह 'सर्वतोमुखः' है अर्थात् उसके मुख सब दिशाओं में हैं।
मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ।।३४ ।।
शब्दार्थ : मृत्युः मृत्यु, सर्वहर: सब का विनाश करने वाला, च-और, अहम् - मैं, उद्भवः -समृद्धि, च-और, भविष्यताम् -समृद्धि प्राप्त करने वालों का , कीर्ति: -कीर्ति, श्रीः -समृद्धि, वाक्-वाणी, , स्मृतिः स्मरण शक्ति, मेधा-बुद्धि, धृति:-दृढ़ता, क्षमा-क्षमा।
अनुवाद : मैं सर्वहर मृत्यु हूँ। समृद्ध होने वालों की समृद्धि हूँ। नारी के गुणों में मैं कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ।
व्याख्या : सर्वस्व नाश करने वाली और सर्वस्व हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ। मृत्यु दो प्रकार की होती है-एक तो धन-वैभव का हरण करने वाली और दूसरी जीवन हरण करने वाली। इन दोनों में जीवन हरण करने वाली मृत्यु सर्वहर मृत्यु कही जाती है। मैं वही हूँ।
दूसरी व्याख्या इस प्रकार है-मैं सर्वहर परम पुरुष हूँ क्योंकि प्रलयकाल में मैं सर्वस्व हरण कर लेता हूँ।
भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी जीवों का मैं उद्भव हूँ। मैं ऐश्वर्य हूँ और उनके लिए ऐश्वर्य प्राप्ति का साधन हूँ जो इसके योग्य हैं।
सौन्दर्य श्री है। कान्ति श्री है। जीवन मे किंचित्मात्र ख्याति प्राप्त कर लेने पर लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त कर ली है और वे बहुत महान् हो गये हैं। मैं न्याय के सिंहासन को विभूषित करने वाली वाक् हूँ। मैं स्मृति हूँ जो भूत्काल के सुखों और विषयों का स्मरण कराती है।
शास्त्रों के उपदेशों को धारण करने वाली बुद्धि मेधा है जो मन की विशेष शक्ति है। कष्टों में भी शरीर और इन्द्रियों को संयत रखने की शक्ति धृति है। कर्म करते समय अनासक्त रहना भी धृति शक्ति के कारण सम्भव है। साहस धृति से होता है। क्षमा सहनशीलता भी है।
कीर्ति, श्री, स्मृति, मेधा और धृति दक्ष की कन्यायें हैं। धर्म के साथ उनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ था अतः वे धर्मपत्नियाँ भी कहलाती हैं।
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ।।३५ ।।
शब्दार्थ : बृहत्साम-बृहत्साम, तथा-और, साम्नाम् -साम श्रुतियों में, गायत्री गायत्री, छन्दसाम् छन्दों में, अहम् -मैं, मासानाम् मासों में, मार्गशीर्षः मार्गशीर्ष, अहम् -मैं, ऋतूनाम्-ऋतुओं में, कुसुमाकरः- वसन्त ऋतु ।
अनुवाद: श्रुतियों में प्रमुख बृहत्साम हूँ, छन्दों में मैं गायत्री हूँ, मासों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में कुसुमाकर (वसन्त) मैं हूँ।
व्याख्या: सामवेद की श्रुतियों में प्रमुख बृहत्साम है। बृहत् का अभिप्राय है बड़ा।
मार्गशीर्ष-दिसम्बर मास के मध्य से जनवरी मध्य तक मार्गशीर्ष माना जाता है। इस मास में जलवायु प्रशान्त और सुखद होती है। प्राचीन काल में वर्ष के मासों की गणना इसी मास से की जाती थी। इस मास को प्रथम स्थान दिया जाता था। कुसुमाकर-सुन्दर पुष्पों की ऋतु वसन्त ।
द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ।।३६ ।।
शब्दार्थ : द्यूतम् - धूत (जुआ), छलयताम् छल करने वालों में, अस्मि (मैं) हूँ, तेजः -तेज, तेजस्विनाम् -तेजस्वियों का, अहम् - मैं, अय-विजय, अस्मि (मैं) हूँ, व्यवसाय:- निश्चय (निश्चय करने वालों का), अस्मि (मैं) हूँ, सत्त्वम् सत्त्व, सत्त्वत्वताम् -सात्त्विक पुरुषों का, अहम् - मैं।
अनुवाद : छल करने वालों में मैं द्यूत (जुआ) हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ, विजय मैं हूँ, निश्चय मैं हूँ, सात्त्विकों का सत्त्वभाव मैं हूँ।
व्याख्या : दूसरों को छलने की विधियों में मैं द्यूत क्रीड़ा हूँ। जूआ मेरी अभिव्यक्ति है। मैं शक्तिवानों की शक्ति हूँ। मैं विजयी की विजय हूँ। प्रयत्न करने वालों का मैं यत्न हूँ।
मैं सात्त्विक पुरुषों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों का सत्त्व हूँ।
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ।।३७ ।।
शब्दार्थ : वृष्णीनाम् वृष्णि वंश में, वासुदेवः - वासुदेव, अस्मि - (मैं) हूँ, पाण्डवानाम् -पाण्डवों में, धनञ्जयः -धनञ्जय, मुनीनाम् -मुनियों में, अपि -भी, अहम् -मैं, व्यासः व्यास, कवीनाम् -कवियों में, (शुक्राचार्य), कविः-कवि । उशनाः-उशना
अनुवाद : वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, पाण्डवों में मैं अर्जुन हूँ, ऋषियों में मैं व्यास हूँ, कवियों में मैं उशना कवि हूँ।
व्याख्या : वृष्णि यादव अर्थात् यदु वंश के वंशज हैं। मैं उनमें अग्रगण्य हूँ।
उशना कवि दैत्यों के आचार्य (गुरु) शुक्राचार्य हैं।
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ।।३८ ।।
शब्दार्थ : दण्डः दण्ड, दमयताम् - दमन करने वालों का, अस्मिㅡ (मैं) हूँ, नीतिः नीति, अस्मि (मैं) हूँ, जिगीषताम् - जीतने की इच्छा रखने वालों की, मौनम्-मौन, च-और, एव-ही, अस्मिㅡ(मैं) हूँ, गुह्यानाम् -रहस्यों में, ज्ञानम्-ज्ञान, ज्ञानवताम् - ज्ञानियों का, अहम् -मैं।
अनुवाद : दण्ड देने वालों का दण्ड मैं हूँ, विजय की आकाङ्क्षा रखने बालों की नीति मैं हूँ, रहस्यों में (गुप्त रखने योग्य विषयों में) मौन मैं हूँ। विद्वानों का ज्ञान मैं हूँ।
व्याख्या : नीति-साम, नीति,
मौनम्-ब्रह्म अथवा आत्मा पर सतत ध्यान के पश्चात् की अवस्था । ज्ञानम् आत्मा का ज्ञान ।
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ।।३९ ।।
शब्दार्थ : यत्-जो, च-और, अपि-भी, सर्वभूतानाम् -सब प्राणियों में, बीजम् बीज, तत्-वह, अहम् -मैं, अर्जुन-हे अर्जुन, न नहीं, तत्-वह, अस्ति-है, विना-विना, यत्-जो, स्यात् -हो, मया-मेरे द्वारा, भूतम् - प्राणी, चराचरम् -चर और अचर (चेतन और जड़)।
अनुवाद : और हे अर्जुन, सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। कोई भी जीव चेतन अथवा जड़, ऐसा नहीं है जो मेरे बिना रह सकता हो ।
व्याख्या : मै समस्त सृष्टि के अस्तित्व का बीज रूप मूल कारण है। मैं सब का बीज है. प्रत्येक पदार्थ का मैं आत्म-तत्त्व हैं। मेरे बिना किसी का अस्तित्व सम्भव नहीं। सब वस्तुएँ मेरी ही प्रकृति की हैं। मैं सब का सार-तत्त्व हूँ। बिना मेरे सर्वस्व शून्य होता है। मैं सब का आत्म-तत्त्व हूँ।
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ।।४० ।।
शब्दार्थ: न-नहीं, अन्तः-अन्त, अस्ति-है, मम्-मेरी, दिव्यानाम् -दिव्य, विभूतीनाम्- विभूतियों का, परंतप -हे शत्रु संहार करने वाले (अर्जुन), एषः यह, तु निश्चित रूप से, उद्देशतः संक्षेप में, प्रोक्त -कहा गया है, विभूतेः-विभूति का, विस्तरः-विस्तार, मया-मेरे द्वारा।
अनुवाद : हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अन्त नहीं है किन्तु यह तो संक्षेप में मैंने तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार बताया कि
व्याख्या : भगवान् की दिव्य विभूतियों का यथार्थ रूप से विस्तार बताना अथवा जानना सर्वथा असम्भव है। भगवान् की शक्तियों अथवा विभूतियों की कोई सीमा नहीं है। उनकी अनन्त महिमा का गुणगान जितना भी करें वह अल्प ही है।
परन्तप-शत्रुओं का संहार करने वाला। परन्तप वह है जो अपने अन्दर के शत्रुओं-काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का विनाश करता है।
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ।।४१ ।।
शब्दार्थ : यद्यत् (यत्, यत्) -जो भी, विभूतिमत् - विभूति युक्त, सत्त्वम् -वस्तु, श्रीमत् -ऐश्वर्य युक्त, ऊर्जितम् - शक्तियुक्त, एव-ही, वा-अथवा, तत् तत्-वह, वह, एव-ही, अवगच्छ-जानो, त्वम्-तुम, मम-मेरे, तेजोंऽशसंभवम् -तेज के अंश से उद्भूत ।
अनुवाद : (संसार में) जो कुछ भी विभूतियुक्त है, ऐश्वर्ययुक्त है, कान्तियुक्त है अथवा शक्तियुक्त है वह सब मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जानो ।
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ।।४२ ।।
शब्दार्थ: अभवा-अथवा, बहुना बहुत (से), एतेन-इससे, शाले जानने से, तब तुम्हारा, अर्जुन हे अर्जुन, का के अहमी, इदम् - यह, कृत्स्नम् -समस्त, एकाशेन-एक अंश से. स्थित-स्थित, जगत् संसार । विष्टभ्य-धारण
अनुवाद: किन्तु हे अर्जुन, इतने विस्तृत ज्ञान को लेने में तुम्हारा क्या प्रयोजन है? समस्त ब्रह्माण्ड को अपनी शक्ति के अंश से धारण कर के में स्थित हैं।
व्याख्या: भगवान् यह कह कर अपनी बात को विराम देते हैं कि वे इस संसार को स्थित कर के उसमें व्याप्त हो कर अपने केवल एक अंश से ही उजम धारणा किये हुए हैं। यह श्लोक ऋग्वेद के पुरुष सूक्त १०.९०.३ की इस घोषणा पर आधारित है- "उसका एक पाद तो यह विश्व की अभिव्यक्ति और तीन पाद द्युलोक में अमृत रूप से स्थित हैं।"
मैं इस संसार को अपने एक अंश अथवा एक पाद से धारण किये हुए हूँ। मेरा एक पाद ही समस्त प्राणी हैं।
समस्त जीव उसके पाद से स्थित हैं (तैत्तिरीय आरण्यक ३.१२)। सम्पूर्ण ससार भगवान् का एक पाद है। हमारे अज्ञान अथवा सीमित बुद्धि के कारण अश अथवा पाद की परिकल्पना की गई है। वस्तुतः ब्रह्म अखण्ड, अव्यय और निराकार है।
अब अर्जुन को भगवान् की विभूतियों का ज्ञान हो गया है। वह भगवान् के अतिशोभन् विभूतिमत् स्वरूप को देखने का अधिकारी हो गया है। भगवान् कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार अपनी विभूतियों का उपदेश कर के उसे महत् दर्शन के लिए तैयार करते हैं।
अर्जुन कहते हैं- "हे भगवन्, अब मैं जान गया हूँ कि सम्पूर्ण जगत् आपसे व्याप्त है। अब मैं दिव्य चक्षु के द्वारा आप में समस्त ब्रह्माण्ड के दर्शन करना चाहता हूँ।"
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ।।
।। इति विभूतियोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथैकादशोऽध्यायः
विश्वरूपदर्शनयोगः
अर्जुन उवाच
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।।१ ।।
शब्दार्थ : मदनुग्रहाय -मुझे आशीर्वाद देने के लिए, परमम् -सर्वोच्च, गुह्यम् -रहस्यात्मक, अध्यात्मसंज्ञितम् - अध्यात्म संज्ञा वाले, यत्-जो, त्वया-आपके द्वारा, उक्तम् -कहे गये, वचः-शब्द, तेन-उससे, मोहः- मोह, अयम् - यह, विगतः नष्ट हो गया, मम-मेरा ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : आपने मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझ पर अनुकम्पा कर के जो परम गोपनीय अध्यात्म ज्ञान के आशीष वचन कहे उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है।
व्याख्या : भगवान् की विभूतियों को श्रवण करने के पश्चात् अर्जुन में भगवान् के अद्भुत विश्वरूप दर्शन की तीव्र अभिलाषा जाग्रत हुई है। उसकी किंकर्तव्यविमूढ़ता और मोह अब नष्ट हो चुके हैं।
अध्यात्म-वह विवेक शक्ति जो आत्मा और अनात्मा का भेद दर्शाती है वह अध्यात्म विद्या है।
अपने ही सम्बन्धियों और आचार्यों का संहार करने में मैं भयभीत था कि कहीं पाप न हो जाये । मैं सोचता था- “उन्हें मारने में मैं ही हेतु हूँ। और वे मेरे द्वारा ही मारे जाने हैं।"
आपका दुर्बोध और अत्यन्त अमोघ उपेदश प्राप्त कर के मेरा मोह समाप्त हो गया है। आपने इस अज्ञान रूपी भ्रम को दूर कर दिया है। विश्वरूप दर्शन आत्यन्तिक लक्ष्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो इसी
अध्याय के साथ ही गीता परिसमाप्त हो जाती । क्रमिक अनुभवों में विश्वरूप दर्शन एक और अनुभव है। यह अनुभव कराल (भीषण) भी है। यही कारण था कि अर्जुन ने स्खलित स्वर में भगवान् से कहा- आपका स्वरूप कितना भीषण (भयावह) है। मैंने वह सब देखा है जो मुझसे पूर्व किसी ने नहीं देखा। भरा चित्त प्रसन्न है पुनरपि भय के कारण व्याकुल है। भगवन्! कृपया मुझे मेरा विसुन्दर-स्वरूप पुनः दिखाओ । हे देवाधिदेव, सर्वाधार, शंख, चक्र, गदा, अपना से में धारण करके मुकुटधारी स्वरूप के दर्शन कराओ। मैं आपको पुनः पूर्व स्वरूप में देखने की अभिलाषा करता हूँ। हे सहस्रबाहो विराट् स्वाम भगवन्, मैं आपका चतुर्भुज स्वरूप देखना चाहता हूँ। आप उसी रूप को धारण करो।
अर्जुन को भगवान् ने अपने उपदेश में कहा था- "अपने एक अंश से इस विश्व को मैंने धारण किया हुआ है।" इसी से अर्जुन को भगवान् के विश्वरूप दर्शन की आकांक्षा हुई। वह कहता है-"हे करुणानिधान, आपने मुझे अध्यात्म ज्ञान दिया जो वेदों में खोजना भी कठिन है। आपने मेरी रक्षा की है। मेरा भ्रम लुप्त हो गया है। आपने अपनी दिव्य विभूतियों, प्रकृति के रहस्यों व परम आत्म-ज्ञान के तत्त्व को मेरे समक्ष रखा है, उन्हें प्रकाशित किया है। इस क्षण मेरी तीव्र उत्कण्ठा यही है कि अपने इन नेत्रों से आपके विश्वरूप दर्शन करूँ।"
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ।।२ ।।
शब्दार्थ : भवाप्ययौ-उत्पत्ति और प्रलय, हि-निश्चित रूप से, भूतानाम् - प्राणियों की, श्रुतौ-श्रवण की गई है, विस्तरशः - विस्तार से, मया-मेरे द्वारा, त्वत्तः- आप से, कमलपत्राक्ष-हे कमल नयन, माहात्म्यम् -महानता, अपि -भी, च-और, अव्ययम् अविनाशी ।
अनुवाद : हे कमलनेत्र भगवान्, निश्चित रूप से मैंने जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में तथा आपकी अविनाशी महिमा को भी, विस्तार से, आपके मुखारविन्द से श्रवण किया है।
व्याख्या: कमल-पत्र के समान नेत्र वालेअथवा वे जिनके नेत्र कमल-पत्र केसमान हों। कमल पत्र का दूसरा अर्थ है- आत्म-ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है वह कमलपत्राक्ष है।
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ।।३ ।।
शब्दार्थ : एवम् - इस प्रकार, एतत् - यह, यथा-जैसे, आत्थ-आपने कहा है, त्वम्-आप, आत्मानम् -स्वयं को, परमेश्वर- हे परमेश्वर, द्रष्टुम् - देखने इच्छा करता हूँ, ते आपका, रूपम् पुरुषोत्तम -हे पुरुष श्रेष्ठ।
अनुवाद : (अब) हे परमेश्वर, आपने अपने ऐश्वर्यशाली स्वरूप का विबरण दे दिया है किन्तु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन की आकाङ्क्षा रखता हूँ।
व्याख्या : कतिपय व्याख्याकारों ने श्लोक के दो स्वतन्त्र भाग कर के इस प्रकार भाव दिया है-
हे परमेश्वर, आपने जो कुछ अपने विषय में कहा है ठीक वैसा ही है। (पुनरपि) हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वर स्वरूप के दर्शन का अभिलाषी हूँ।
रूपमैश्वरम् - आपका स्वरूप, ईश्वर रूप में, विष्णु रूप में जो अनन्त ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, पराक्रम और तेज से युक्त है।
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयाऽत्मानमव्ययम् ।।४ ।।
शब्दार्थ : मन्यसे आप सोचते हैं (मानते हैं), यदि यदि, तत्-वह, शक्यम् -सम्भव, मया-मेरे द्वारा, द्रष्टुम् -देखना, इति-इस प्रकार, प्रभो-हे प्रभु, योगेश्वर- हे योगियों के ईश्वर, ततः-फिर, मे-मुझे, त्वम् - आप, दर्शय-दिखाओ, आत्मानम् – (अपना) स्वरूप, अव्ययम् अविनाशी ।
अनुवाद : हे प्रभो, यदि आप मानते हैं कि मैं आपका स्वरूप देखने का अधिकारी हूँ तो हे योगेश्वर, मुझे अपना अविनाशी स्वरूप दिखाइये।
व्याख्या : भगवान् के विश्वरूप दर्शन के लिए अर्जुन अत्यन्त उत्सुक और अभीप्सित है। वह उनसे दर्शनार्थ प्रार्थना करता है। उन्हीं की अहेतुकी अनुकम्पा से यह दर्शन सम्भव है।
योगेश्वरः योग का स्वामी-यह भाव भी हो सकता है। योगी वह है जो आठ आध्यात्मिक सिद्धियों से युक्त है। योगियों का स्वामी योगेश्वर है। साधक पर इस एकत्व प्रसाद की वृष्टि करने में सक्षम योगी, योगेश्वर हरिय व्यष्टि आत्मा का समष्टि आत्मा से एकत्व योग है। अधिकारी आध्यात्मिक जो सृष्टि, स्थिति, संहार, आवरण और कृपापूर्वक विमुक्त करने में सक्षम है वह भगवान् है। (ये पंच क्रियायें क्रमशः सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह से भी संज्ञित हैं अर्थात् जानी जाती हैं।)
श्री भगवानुवाच
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।।५ ।।
शब्दार्थ : पश्य -देखो, मे मेरे, पार्थ-हे पार्थ, रूपाणि-रूप. शतशः शत-शत (सैकड़ों), अथ और, सहस्रशः सहस्रों (हजारों), नानाविधानि अनेक प्रकार के, दिव्यानि -दिव्य, नानावर्णाकृतीनि - विविध वर्ण और आकार वाले, च-और।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : हे अर्जुन, मेरे दिव्य, विविध प्रकार के, विविध वर्ण और आकार वाले सैकड़ों हजारों रूपों को देखो।
व्याख्या : दिव्यानि-दिव्य, अलौकिक ।
शतशः, सहस्रशः- सैकड़ों, हजारों-अनन्त, अगणित ।
हे अर्जुन, मैं तुम्हें विश्वरूप दिखाना चाहता हूँ। समस्त प्राणी और भाव (अस्तित्व) उसमें निहित हैं। मोटे और दुबले, (कद में) छोटे और लम्बे, लाल और काले, पुरुषार्थी और आलसी, धनी और निर्धन, बुद्धिमान् और मूढ़, स्वस्थ और रोगी, शान्त और अशान्त, जाग्रत और सुषुप्त, सुन्दर और कुरूप, और समस्त स्तरों के प्राणी अपने विशेष लक्षणों से युक्त तुम देखोगे । आकाश का नीलवर्ण, सिल्क का पीतवर्ण, संध्याकाल का रक्तवर्ण, कोयले का श्यामवर्ण, बर्फ का श्वेतवर्ण ओर पत्तों का हरितवर्ण तुम देखोगे । तुम विभिन्न आकार के पदार्थ भी देखोगे ।
पश्यादित्यान्वसूतद्रानश्विनी मरुतस्तथा ।
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याऽश्चर्याणि भारत ।।६ ।।
शब्दार्थ : पश्य-देखो, आदित्यान् - आदित्यों को, यसून वसुओं को, रुद्रान् रुद्रों को, अश्विनी-दो अश्विनी कुमारों को, मरुतः मस्तों को, सधको, और, बहूनि अनेक, अदृष्टपूर्वाणि-पहले न देखे हुए, पश्य-देखो, आश्चर्याणि - आश्चयों को, भारत-हे भारत ।
अनुवाद : हे अर्जुन, आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, दो अश्विनी कुमारों को और मरुतों को देखो। अनेक पहले न देखे हुए आश्चयों को देखो।
व्याख्या : पूर्व अध्याय में आदित्यों, वसुओं, रुद्रों और मरुद्गणों का वर्णन आ चुका है।
इतना ही नहीं, अनेक ऐसे आश्चर्यों को देखो जो न तो तुमने कभी पहले देखे और न ही किसी और ने देखे।
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि ।।७ ।।
शब्दार्थ : इह-यहाँ, एकस्थम् - एक में स्थित, जगत्-जगत्, कृत्स्नम् -पूर्ण, पश्य-देखो, अद्य-आज, सचराचरम् -चर और अचर सहित, मम-मेरे, देहे देह में, गुडाकेश - हे गुडाकेश (अर्जुन), यत्-जो, अन्यत् अन्य, द्रष्टुम् - देखना, इच्छसि चाहते हो।
अनुवाद : हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में चराचर सहित समस्त ब्रह्माण्ड को एक ही स्थान में स्थित देखो। अन्य जो कुछ देखने की इच्छा रखते हो, वह भी देखो।
व्याख्या : अन्यत्-अन्य जो कुछ भी अर्थात् तुम्हारी विजय अथवा पराजय, जिसके विषय में तुम्हारे मन में सन्देह है। (निरूपण-11.6)
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ।।८।।
शब्दार्थ : न - नहीं, तु-किन्तु, माम् -मुझे, शक्यसे-(तुम) शक्य हो, समर्थ हो, द्रष्टुम् - देखने में, अनेन-इस के द्वारा, एव-ही, स्वचक्षुषा-अपने नेत्रों, दिव्यम् - दिव्य, ददामि देता हूँ, ते तुम्हें, चक्षुः नेत्र, पश्य-देखो, मे-मेरे, योगम् योग को, ऐश्वरम् - ऐश्वर्यशाली ।
अनुवाद : किन्तु अपने इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति के दर्शन करो।
व्याख्या : इन भौतिक नेत्रों से कोई मेरे वैश्विक स्वरूप को नहीं देख सकता । इसे तो अलौकिक (दिव्य) नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। इसे मन की आँख से देखने का भ्रम नहीं होना चाहिए। यह एक अनुभूति है।
भगवान् कृष्ण अर्जुन से कहते हैं- "मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिससे तुम मेरे ब्रह्माण्डीय रूप के दर्शन कर सकते हो। इस के द्वारा मेरी अद्भुत यौगिक शक्ति को देखो।"
अनेन इसके द्वारा-मांसल अथवा स्थूल भौतिक नेत्र। (निरूपण-VII.25; IX.5; Χ.7)
सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ।।९ ।।
शब्दार्थ : एवम् - इस प्रकार, उक्त्वा-कह कर, ततः-फिर, राजन् -हे राजन्, महायोगेश्वरः योग के महान् स्वामी (कृष्ण), हरिः- हरि, दर्शयामास- दिखाया, पार्थाय पार्थ को, परमम् -परम, रूपम् -रूप, ऐश्वरम् -ऐश्वर्यशाली।
सञ्जय ने कहा
अनुवाद : हे राजन्, ऐसा कह कर योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यशाली ईश्वरीय स्वरूप दिखाया।
व्याख्या : राजन् यह श्लोक संजय द्वारा राजा धृतराष्ट्र को सम्बोधित है।
परमं रूपम् - विश्वरूप ।
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ।।१० ।।
शब्दार्थ : अनेकवक्त्रनयनम् -अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेकाद्भुतदर्शनम् - अनेक अद्भुत दृश्यों से युक्त, अनेकदिव्याभरणम् - अनेक दिव्य आभूषणें से युक्त, दिव्यानेकोद्यतायुधम् - अनेक दिव्य शस्त्रों को धारण किये हुए।
अनुवाद : अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दृश्यों से युक्त, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्र धारण किये हुए (ऐसा स्वरूप उन्होंने दिखाया)।
व्याख्या : अगणित वदन प्रत्यक्ष हुए। अर्जुन ने इस विश्वरूप को पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त देखा। समस्त अभिव्यक्ति भगवान् का एक विशाल स्वरूप सी थी। भगवान् ही सब कुछ थे, ऐसा अर्जुन ने देखा।
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ।।११ ।।
शब्दार्थ : दिव्यमाल्याम्बरधरम् - दिव्य माला और आभरण (वस्त्र) धारण किये हुए, दिव्यगन्धानुलेपनम् - दिव्य गन्ध का अनुलेप किये हुए, सर्वाधर्यमयम् -सब प्रकार से अद्भुत, देवम्- (देदीप्यमान्) देव को, अनन्तम्-अनन्त, विश्वतोमुखम् -सब ओर मुख वाले।
अनुवाद : दिव्य माला और वस्त्र धारण किये हुए, (शरीर पर) दिव्य गन्ध का अनुलेप किये हुए, सब प्रकार से अद्भुत, देदीप्यमान्, अनन्त और सब ओर मुख वाले (भगवान् को अर्जुन ने देखा) ।
व्याख्या : विश्वतोमुखम् -सब ओर मुख वाले क्योंकि समस्त प्राणियों की अन्तरात्मा वे स्वयं हैं।
देवम्-देवता (भगवान्), देदीप्यमान् ।
अनन्तम्-सीमारहित । देश-काल-वस्तु परिच्छेद, इन तीन प्रकार की सीमाओं से जो मुक्त है। वह ब्रह्म ही है। इस दार्शनिक विचारधारा को निम्न प्रकार से समझाया गया है-
पात्र यहाँ है-यह देश की सीमा है।
पात्र अब यहाँ है यह काल की सीमा है।
पात्र वस्त्र नहीं है-यह पदार्थ (वस्तु) की सीमा है।
कुंकुम केवल कश्मीर में है-यह देश-वस्तु परिच्छेद है।
तुम केवल सितम्बर में सेब प्राप्त कर सकते हो-यह काल-वस्तु परिच्छेद है।
किन्तु ब्रह्म सर्वत्र है क्योंकि वह सर्वव्यापक है। वह भूत, वर्तमान और भविष्यत तीनों कालों में रहता है। वह सब खण्डों में रहता है। इसलिए वह (देश-काल-वस्तु की) सीमाओं से अतीत है और अतीत होने से अनन्त स्वरूप है।
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ।।१२ ।।
शब्दार्थ : दिवि-आकाश में, सूर्यसहस्रस्य-एक सहस्र सूर्यों की, भवेत् -हो, युगपत् - एक साथ, उत्थिता-उदित, यदि यदि, भाः-तेज, सदृशी समान, सा-वह, स्यात्-हो, भासः-तेज, तस्य-उस, महात्मनः- (महान् आत्मा) विशाल पुरुष का ।
अनुवाद : आकाश में यदि एक सहस्र सूर्यों का तेज एक साथ प्रकाशित तो वह भी तेज कदाचित् ही उस महान् विश्वरूप पुरुष के सदृश हो ।
दिवि- अन्तरिक्ष अथवा आकाश ।
महात्मा-महान् आत्मा, विशाल पुरुष अथवा विश्वरूप।
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ।।१३ ।।
शब्दार्थ : तत्र-वहाँ, एकस्थम् - एक में स्थित, जगत् ब्रह्माण्ड, कृत्स्नम् -सम्पूर्ण, प्रविभक्तम् -विभक्त, अनेकधा अनेक समूहों में, अपश्यत् देखा, देवदेवस्य -देवों के देव के, शरीरे-शरीर में, पाण्डवः -पाण्डु पुत्र (अर्जुन), तंदा-फिर ।
अनुवाद : वहाँ अर्जुन ने देवाधिदेव कृष्ण के शरीर में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अनेक समूहों में विभक्त एक ही स्थान में स्थित देखा।
व्याख्या: तत्र-वहाँ विश्वरूप में।
अनेकधा-अनेक समूह-देव, पितर, मनुष्य और जीवों की अन्य जातियाँ।
अर्जुन ने सब रूपों को भगवान् के रूपों में देखा। सब सिर उनके सिर, सब नेत्र उनके नेत्र, सब हाथ उनके हाथ, सब पाँव उनके पाँव, प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अङ्ग मानो भगवान् के शरीर का ही अङ्ग हो, उनके स्वरूप का ही अंश हो। जहाँ भी वह देखता भगवान् ही दृष्टिगोचर होते। उसने रहस्यपूर्ण गोपनीय दिव्य ज्ञान प्राप्त किया।
संजय ने विश्वरूप का वास्तव में स्पष्ट चित्रण किया है। पुनरपि, सीमित मन से इसे ग्रहण करना व्यर्थ है। यह भावांतीत (अलौकिक) दर्शन है जो मन और इन्द्रियों की पहुँच से परे है। इसे तो समाधि में साक्षात्कार किया जा सकता है।
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ।
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ।।१४ ।।
शब्दार्थ : ततः तब, सः- वह, विस्मयाविष्टः- आश्चर्यचकित हो कर, कश्रोमा-पुलकित (रोमांचित) शरीर, धनञ्जयः-अर्जुन, प्रणम्य-प्रणाम करके, शिरसा-सिर से, देवम्-भगवान् को, कृताञ्जलिः- हाथ जोड़ कर, अभाषत-बोला ।
अनुवाद : तत्पश्चात् आश्चर्य से अभिभूत हो कर और रोमांचित हो कर अर्जुन ने सिर झुका कर भगवान् को प्रणाम किया और करबद्ध होकर बोला।
व्याख्या : ततः-तत्पश्चात्, विश्वरूप दर्शन के उपरान्त ।
विश्वरूप को दण्डवत् प्रणाम करने के लिए अर्जुन ने हाथ जोड़े। करबद्ध होना और सिर झुकाना इस बात के द्योतक हैं कि वीर अर्जुन में विनयशीलता आ गई थी जो भक्तिभाव के मुख्य लक्षण हैं।
अर्जुन उवाच
पश्यामि देवांस्तव देव देहे
सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ-
मृर्षीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ।।१५ ।।
शब्दार्थ : पश्यामि-देखता हूँ, देवान्-देवों को, तव-आपके, देव-हे भगवन्, देहे-देह में, सर्वान् -समस्त, तथा-और, भूतविशेषसङ्घान् - विशेष प्राणियों के समूहों को, ब्रह्माणम्-ब्रह्मा को, ईशम् - भगवान् को, कमलासनस्थम् -कमल पर विराजित, ऋषीन्-ऋषियों को, च-और, सर्वान् समस्त, उरगान् -सपों को, च-और, दिव्यान् - दिव्य ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे भगवन्, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं और विविध जातियों के प्राणी समुदायों को देख रहा हूँ। कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा तथा समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ।
व्याख्या : विश्वरूप दर्शन का वर्णन, अर्जुन अपने अनुभव के आधार पर इस श्लोक में तथा आगे के श्लोकों में (१५ से ३१ तक) कर रहे हैं।
भूतविशेषसङ्घान्-चर और अचर विविध प्रकार के भूत समुदाय। रोमवत् ये अगणित सत्तायें आपके शरीर में हैं।
सब जीवों के स्वामी चतुर्मुख ब्रह्मा मेरु पर्वत पर धरा-कमल के मध्य में आसनस्थ हैं जो धरा-कमल के भीतरी कक्ष के समान हैं।
ऋषि-वसिष्ठ आदि ऋषि, उरगान् वासुकि आदि सर्प ।
और भी...
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।। १६ ।।
शब्दार्थ : अनेकबाहूद्रवक्त्रनेत्रम् अनेक भुजा, उदर, मुख और नेत्रों सहित, पश्यामि देखता हूँ, त्वाम्-आपको, सर्वतः सब ओर, अनन्तरूपम् - अनेक रूप वाले, न नहीं, अन्तम् अन्त, न नहीं, मध्यम् -मध्य, न-नहीं, पुनः पुनः, तव-आपका, आदिम् - आदि, पश्यामि देखता हूँ, विश्वेश्वर- हे संसार के स्वामी, विश्वरूप-विश्वरूप ।
अनुवाद : हे विश्वरूप विश्वेश्वर, मैं आपको सर्वतः (सब ओर) अनेक भुजा, उदर, मुख और नेत्रों सहित अनन्त रूपों में देख रहा हूँ किन्तु भगवन् न तो मुझे आदि, न मध्य और न ही अन्त दिखाई दे रहा है।
व्याख्या : सीमित देश-काल में वस्तु का आदि, मध्य और अन्त होता है किन्तु भगवान् सर्वव्यापक और शाश्वत हैं। वे भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों में रहते हैं किन्तु देश-काल के बन्धन से अतीत हैं। इसीलिए उनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है।
भगवान् द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षु के कारण ही अर्जुन इस दिव्य-स्वरूप के दर्शन कर सके। भगवान् के प्रति जो परम प्रीति रखता हो और जिन पर भगवान् अपनी कृपा-दृष्टि करें वही इस अद्भुत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है।
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- द्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ।।१७ ।।
शब्दार्थ : किरीटिनम् -मुकुटयुक्त, गदिनम् - गदायुक्त, चक्रिणम् - चक्रयुक्त, च-और, तेजोराशिम् - तेजपुञ्ज से युक्त, सर्वतः सब ओर, दीप्तिमन्तम् देदीप्यमान्, पश्यामि देखता हूँ, त्वाम् - आपको, दुर्निरीक्ष्यम् - जिसे देख पाना भी कठिन है, समन्तात् - चारों ओर, दीप्तानलार्कद्युतिम् - धधकती आग और देदीप्यमान् सूर्य के समान, अप्रमेयम्-अप्रमेय, अपरिमित ।
अनुवाद : मैं आपको सर्वत्र मुकुट, गदा और चक्र से युक्त प्रकाशमान तेज पुंज के रूप में देख रहा हूँ जो कठिनता से देखने योग्य है और प्रदीप्त अग्नि और देदीप्यमान् सूर्य के समान ज्योतिर्मय तथा अप्रमेय है।
व्याख्या : किरीटिन सिर के लिए एक विशेष आभूषण मुकुट है।
अर्जुन ने भगवान् की मुकुट, गदा और चक्र युक्त स्वरूप में पूजा की थी अतः भगवान् ने वही स्वरूप दिखाया। सर्वातिरिक्त अलौकिक सत्य तो यह है कि भगवान् सब रूपों में हैं और सब रूपों से अतीत हैं। उनकी महिमा को कौन समझ सकता है?
तेजोराशिम् - तेजपुञ्ज, जो दिव्य चक्षु से ही देखना सम्भव है। अप्रमेयम्-अपरिमित, जिसकी सीमा नहीं बांधी जा सकती।
आपकी योग शक्ति के दर्शन से मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप विष्य, वर्तमगर अविनाशी हैं, अनन्त हैं, अप्रमेय हैं आदि आदि।
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।।१८ ।।
शब्दार्थ : त्वम् आप, अक्षरम् - अक्षर (अविनाशी), परमम् -परम, बेदितव्यम् - जानने योग्य, त्वम् -आप, अस्य-इस, विश्वस्य-विश्व के, परम् -महान्, निधानम् आश्रय, त्वम्-आप, अव्ययः अविनाशी, शाश्वतधर्मगोप्ता-शाश्वत धर्म की रक्षा करने वाले, सनातनः-सनातन, त्वम् - आप, पुरुषः पुरुष, मतः मत, मे मेरा ।
अनुवाद : आप अविनाशी हैं, परम पुरुष हैं, जानने योग्य हैं। इस विश्व के आप ही सर्वाधार हैं, शाश्वत धर्म के अमर रक्षक आप ही हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है।
व्याख्या : विश्वस्यनिधानम्-इस विश्व का आधार अथवा विश्राम स्थल । इसी कारण से संसार के समस्त प्राणियों का रक्षण और पोषण होता है। वह अक्षय स्रोत है जिसकी ओर भक्त सभी काल में पहुँचता है। वस्तुतः भ्रमित हैं वे लोग जो इस दिव्य निधान की उपेक्षा कर के विषय-वासनाओं के प्रतिबिम्ब की ओर भागते हैं जो किंचित् मात्र भी सुख प्रदान करने में अक्षम है।
वेदितव्यम् श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा साधक और मुमुक्षु जिसे जान सकते हैं।
अव्ययः-अक्षय, अविनाशी, अपरिवर्तनशील ।
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-
मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ।।१९ ।।
शब्दार्थ : अनादिमध्यान्तम् -आदि, मध्य और अन्त रहित, अनन्तवीर्यम् अनन्त शक्ति से युक्त, अनन्तबाहुम् - अनन्त भुजा वाले, शशिसूर्यनेत्रम् -सूर्य और चन्द्रमा जिनके दो नेत्र हों, पश्यामि देखता हूँ, त्वाम् - आपको, दीप्तहुताशवक्त्रम् - प्रज्वलित अग्नि की भाँति (आपका) मुख, स्वतेजसा-अपने तेज से, विश्वम् - विश्व को, इदम् - यह, तपन्तम् -तपाते हुए।
अनुवाद : मैं आपको आदि, मध्य और अन्त रहित, अनन्त शक्ति से युक्त, अनन्त भुजाओं वाले, सूर्य और चन्द्र रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले, अपने तेज से समस्त ब्रह्माण्ड को तपाते हुए देख रहा हूँ।
व्याख्या : अनन्त बाहु-अनन्त भुजाओं से युक्त अर्थात् उनके अवयवों की परिगणना अनन्त है।
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।
दृष्ट्वाऽद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ।।२० ।।
शब्दार्थ : द्यावापृथिव्योः - भूलोक और स्वर्गलोक के, इदम् - यह, अन्तरम् - मध्य का आकाश, हि-वस्तुतः, व्याप्तम् -पूर्ण, त्वया-आप से, एकेन-एक से, दिशः-दिशायें, च-और, सर्वाः-सब, दृष्ट्वा देख कर,अद्भुतम् -अद्भूत, रूपम् -रूप, उग्रम् उग्र, तव-आपका, इदम् - यह, लोकत्रयम् - तीनों लोक, प्रव्यथितम् - भय से काँप रहे हैं, महात्मन् - हे महात्मन् ।
अनुवाद : भूलोक और स्वर्गलोक के मध्य अन्तरिक्ष तथा सब दिशायें केवल आप से ही पूर्ण हो गई हैं। हे महात्मन्, आपके इस अद्भुत एवं भीषण स्वरूप को देख कर तीनों लोक भय से काँप रहे हैं।
व्याख्या : त्वया-आपके विश्वरूप में।
अन्तरं दिशश्च-यह इस बात का संकेत है कि भगवान् ने विश्व के जड़ और चेतन सभी पदार्थों को अपने स्वरूप से पूर्ण कर दिया था।
द्वितीय अध्याय श्लोक ६ में अर्जुन ने अपनी सफलता के विषय में जो सन्देह किया था उसका निवारण करने के लिए भगवान् कृष्ण उसे अब अनुभव कराते हैं कि पाण्डवों की विजय निश्चित है। (निरूपण -11.6)
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति
केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ।।२१ ।।
शब्दार्थ : अमी-ये, हि-निश्चयेन, त्वाम् आपको, सुरसद्धाः देव समुदाय, विशन्ति-प्रवेश करते हैं, केचित् -कुछ, भीताः- भय में, प्राज्ञ्जलयः-करबद्ध, गृणन्ति-स्तुति करते हैं, स्वस्ति-शुभ हो (कल्याण हो), इति- इस प्रकार, उक्त्वा कह कर, महर्षिसिद्धसङ्घाः- महर्षियों और सिद्धों के समूह, स्तुवन्ति-स्तुति करते हैं, त्वाम् आपकी, स्तुतिभिः-स्तोत्रों से, पुष्कलाभिः पूर्ण, उत्तम ।
अनुवाद : निश्चित रूप से देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ करबद्ध हो कर भय में आप की स्तुति कर रहे हैं, महर्षियों और सिद्धों के समूह 'कल्याण हो' ऐसे वचन कह कर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आप का गुणगान कर रहे हैं।
व्याख्या : पुष्कलाभिः का अभिप्राय है पूर्ण अथवा सुन्दर शब्दों में स्तुति अथवा ऐसी स्तुति जिसमें गहन अर्थ निहित हो।
नारद आदि महर्षि और कपिल आदि सिद्ध प्रेरक स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं।
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ।। २२ ।।
शब्दार्थ : रुद्रादित्याः -रुद्र और आदित्य, वसवः वसु, ये जो, च और, साध्याः साध्य देव, विश्वे-विश्वेदेवा, अश्विनौ-दो अश्विन, मरुतः- मरुत, च-और, उष्मपाः- पितर, च-और, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध समुदाय, वीक्षन्ते-देख रहे हैं, त्वाम् आपको, विस्मिताः- विस्मित हो कर, आश्चर्यचकित हो कर, च-और, एव-ही, सर्वे सब ।
अनुवाद : रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुद्गण, पितर, गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध समुदाय, सभी अत्यन्त आश्चर्य से आपको देख रहे हैं।
व्याख्या : साध्य एक देवों का समुदाय है जिनके प्रमुख ब्रह्मा हैं। विश्वेदेव, दस देव हैं जो वैदिक काल में मानव जाति के रक्षक माने जाते थे। वे संसार के अभिभावक माने जाते थे। मानवों को प्रचुरता में देने वाले वे देव थे।
उनके नाम हैं-क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काम, कल, ध्वनि, रोचक, अद्रव और पुरुरवा ।
दो अश्विनीकुमार प्रभा (विद्युत्) से उत्पन्न हैं और (प्रभा तुष्टा और सूर्य की पुत्री हैं), वे देवों के वैद्य हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और मरुद्गण के विषय में दशम अध्याय के श्लोक २१ और २३ देखें।
उष्मपाः- एक पितर समुदाय । श्राद्धकाल में अर्पित किया गया भोजन ये स्वीकार करते हैं। उन दिनों उष्णता होती है अतः वे उष्मपा कहलाते हैं। पितरों के सात समुदाय हैं।
गन्धर्व-स्वर्गलोक के गायक हैं जैसे हाहा (Haha) हुहु (Huhu) ।
यक्ष-कुबेर, धन-सम्पत्ति के देव । असुर-विरोचन ।
सिद्ध-कपिल ।
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं
महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।
बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम् ।।२३ ।।
शब्दार्थ : रूपम् -रूप, महत्-अपरिमित, ते-आपका, बहुवक्त्रनेत्रम् -अनेक मुख और नेत्रों सहित, महाबाहो - हे महाबाहो, बहुबाहूरुपादम् - अनेक बाहु, उरु (जङ्घा) और पाद से युक्त, बहूदरम् - अनेक उदर वाले, बहुदंष्ट्राकरालम् - अनेक दाँतों से भयानक, दृष्ट्वा देख कर, लोकाः लोक, प्रव्यथिताः- भयभीत हैं, तथा-वैसे ही, अहम् मैं।
अनुवाद : हे महाबाहो! आपके इस अनन्त मुख और नेत्रों वाले, अनेक भुजा और जंघा तथा पाद वाले, अनके उदर और विकराल दाँतों वाले इस अप्रमेय रूप को देखकर लोक भयभीत हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ।
व्याख्या : लोकाः- विश्व - विश्व में रहने वाले समस्त प्राणी। मेरे भय का कारण यह है। अब अर्जुन विश्वरूप की प्रकृति का वर्णन करते हैं जिसके कारण उसका हृदय भय से विदीर्ण हुआ।
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्ण
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ।।२४ ।।
शब्दार्थ : नभःस्पृशम् - आकाश को स्पर्श करते हुए, दीप्तम् - देदीप्यमान, अनेकवर्णम् बहुत वर्णों में, व्यात्ताननम् -विस्तीर्ण (खुले) मुख वाले, दीप्तविशालनेत्रम् -प्रदीप्त विशाल नेत्रों वाले, दृष्ट्वा देखकर, हि-निश्चित रूप से, त्वाम् - आपको, प्रव्यथितान्तरात्मा-हृदय से भयभीत, धृतिम्-धैर्य, ननहीं, facfi - 3MH करता हूँ, शमम्-शान्ति, च-और, विष्णो-हे विष्णो ।
अनुवाद : आकाश को स्पर्श करने वाले, अनेक रङ्गों में चमकते हुए, खुले हुए विस्तीर्ण मुख वाले, विशाल आग्नेय नेत्रों वाले आपके वैश्विक स्वरूप को देख कर, हे विष्णो, मेरा अन्तरात्मा भयभीत हो रहा है। न तो मुझे धैर्य (साहस) मिल रहा है और न ही शान्ति मिल रही है।
व्याख्या : धृति का अभिप्राय सहनशीलता और शक्ति भी है। शम, संयम के भाव में भी प्रयोग किया जा सकता है। विश्वरूप ने अर्जुन को अत्यन्त भयभीत कर दिया है।
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। २५ ।।
शब्दार्थ : दंष्ट्राकरालानि-दाड़ों के कारण भयावह, च-और, ते आपके, मुखानि-मुख, दृष्ट्वा देख कर, एव-ही, कालानलसन्निभानि - प्रलय की आग के समान प्रज्वलित, दिशः-दिशायें, न-नहीं, जाने-जानता, न-नहीं, लभे—प्राप्त करता हूँ, च-और, शर्म-शान्ति, प्रसीद-दया करो (प्रसन्न हों), देवेश- हे देवेश, जगन्निवास-हे विश्वाधार ।
अनुवाद : हे देवेश, हे जगदाधार, दाड़ों के कारण विकराल और प्रलय की अग्नि के समान चमकते हुए आपके मुखों को देख कर मैं दिशाओं का ज्ञान नहीं कर पा रहा हूँ और न ही मुझे शान्ति का आभास हो रहा है। दया करो भगवन्, प्रसन्न हो जाओ।
व्याख्या : जगन्निवास-जगत् का अवलम्बन ।
कालानल-आत्यन्तिक प्रलय की अग्नि जो ब्रह्माण्डों को निगल नेती है। काल (समय) सभी अभिव्यक्त वस्तुओं को विलीन कर देता है। दिशो न जाने-मैं दिशाओं को नहीं देख पा रहा हूँ। प्राची, उदीची (उत्तर), प्रतीची (पश्चिम) और दक्षिण दिशाओं का ज्ञान करने में असमर्थ हूँ।
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः
सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः ।
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ।।२६ ।।
शब्दार्थ : अमी-ये, च-और, त्वाम् - आपको, धृतराष्ट्रस्य- धृतराष्ट्र के, पुत्राः पुत्र, सर्वे-सब, सह-साथ, एव-भी, अवनिपालसङ्घः- नृप समुदाय के साथ, भीष्म:-भीष्म, द्रोण:-द्रोण, सूतपुत्रः-कर्ण, तथा-और, असौ-वह, सह-साथ, अस्मदीयैः- हमारे, अपि-भी, योधमुख्यैः - मुख्य योद्धाओं के साथ ।
अनुवाद : राजाओं के समूह सहित धृतराष्ट्र के सब पुत्र, भीष्म, द्रोण और कर्ण और हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं सहित,
व्याख्या : कर्ण, पाण्डवों की माताश्री कुन्ती का पुत्र था। उसका पालन-पोषण एक सूत (सारथि) ने किया अतः वह उसका पुत्र कहलाया।
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु
संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ।।२७ ।।
शब्दार्थ : वक्त्राणि-मुख, ते-आपके, त्वरमाणा :- शीघ्रता से, विशन्ति-प्रवेश कर रहे हैं, दंष्ट्राकरालानि-भयानक दाँतों वाले, भयानकानि-देखने में भयानक, केचित् -कुछ, विलग्ना:- फँसे हुए, दशनान्तरेषु दाँतों के मध्य रिक्त स्थान में, संदृश्यन्ते देखे जा रहे हैं, चूर्णितैः- चूर-चूर हुए, उत्तमाङ्गैः- उनके सिर सहित।
अनुवाद : कुछ शीघ्रता से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं जो विकाराल दाँतों के कारण देखने में भयानक हैं। अन्य कुछ दाँतों के मध्य फँसे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके सिर चूर-चूर हो चुके हैं।
व्याख्या : वे मुख में किस प्रकार प्रवेश करते हैं ? अर्जुन आगे इसका वर्णन कर रहे हैं।
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः
समुद्रमेवाभिमुखाः द्रवन्ति ।
तथा तवामी नरलोकवीरा
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।। २८ ।।
शब्दार्थ : यथा-जैसे, नदीनाम् नदियों के, बहवः बहुत, अम्बुवेगाः जल प्रवाह, समुद्रम् -समुद्र को, एव -ही, अभिमुखा:- ओर, द्रवन्ति-बहते हैं, तथा वैसे, तव-आपके, अमी-ये, नरलोकवीराः नर लोक के बीर, विशन्ति-प्रवेश करते हैं, वक्त्राणि-मुख, अभिविज्वलन्ति-जलते हुए।
अनुवाद : जिस प्रकार नदियों की वेगपूर्ण धारायें समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं उसी प्रकार नरलोक के ये वीर प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।
व्याख्या : अमी-भीष्म आदि योद्धा । अर्जुन जिन योद्धाओं को मारना नहीं चाहता था उन्हें अब मौत के मुख में जाता देख रहा है। उसका मोह नष्ट हो गया है। अब वह सोचता है- "इस युद्ध का परिहार (त्याग) नहीं हो सकता । परम पुरुष की अनुभूति से यह हो रहा है। अपरिहार्य के लिए मैं चिन्ता क्यों करूँ ? भगवान् ने तो पूर्व से ही इन योद्धाओं को मार दिया है। मैं उनके हाथ का एक खिलौना हूँ। मैं यदि उन्हें मार भी दूँ तो कोई पाप मुझे छू नहीं सकता। यह न्यायपूर्ण कारण भी है।"
क्यों और कैसे वे प्रवेश करते हैं? अर्जुन कहते हैं-
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।
तथैव नाशाय विशन्ति लोका-
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ।।२९ ।।
शब्दार्थ : यथा-जैसे, प्रदीप्तम् - ज्वलित, ज्वलनम् अग्नि, पतङ्गाः-पतङ्गे, विशन्ति-प्रवेश करते हैं, नाशाय-विनाश के लिए, समृद्धवेगाः -अति वेग से, तथा-वैसे ही, एव-ही, नाशाय-विनाश के लिए, विशन्ति-प्रवेश करते हैं, लोकाः -प्राणी, तव-आपके, अपि - भी , वस्त्राणि-मुख, समृद्धवेगाः- अत्यन्त वेग पूर्वक ।
अनुवाद : जिस प्रकार (मोह वश) पतङ्गे अपने ही विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में अत्यन्त वेग से प्रवेश करते हैं उसी प्रकार ये प्राणी अपने विनाश हेतु अत्यन्त वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-
ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ध्वलद्भिः ।
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ।। ३० ।।
शब्दार्थ : लेलिह्यसे-चाट रहे हो, प्रसमानः-निगलते हुए, समन्तात् -सब और से, लोकान् लोकों को, समग्रान् -समस्त, वदनैः- मुखों से, ज्वलद्भिः - जलते हुए (प्रज्वलित), तेजोभिः तेज से, आपूर्य पूर्ण कर के, जगत् संसार, समग्रम् -समस्त, भासः-किरणें, तव-आपके, उग्राः - भयानक, प्रतपन्ति-तप रहे हैं, विष्णो-हे विष्णो।
अनुवाद : हे विष्णो, आप अपने प्रज्वलित मुखों से सब ओर से, समस्त लोकों को निगलते हुए चाट रहे हो। आपके तेज की किरणें सम्पूर्ण जगत् को प्रकाश से पूर्ण करके तपा रही हैं।
व्याख्या : विष्णु-सर्वव्यापक, व्यापनशील ।
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ।।३१ ।।
शब्दार्थ : आख्याहि-बताओ, मे-मुझे, कः-कौन (हो), भवान् - आप, उग्ररूपः- उग्र रूप वाले, नमः -प्रणाम, अस्तु-हो, ते-आपको, देववर-हे देव वर, प्रसीद-दया करो, विज्ञातुम् - जानने के लिए, इच्छामि-इच्छा करता हूँ, भवन्तम् -आपको, आद्यम् - आदि सत्ता, न-नहीं, हि-निश्चित रूप से, प्रजानामि जानता हूँ, तव-आपकी, प्रवृत्तिम् -प्रवृत्ति (कार्य कलाप) को।
अनुवाद : उग्र रूप वाले आप कौन हो, मुझे बताओ । हे देवों में श्रेष्ठ, आपको प्रणाम हो। दया करो। मैं आपको, आदि पुरुष को जानने का इच्छुक हूँ। वास्तव में आपके क्रिया कलापों से अनभिज्ञ हूँ।
श्री भगवानुवाच
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।।३२ ।।
शब्दार्थ : कालः-समय, अस्मि (मैं) हूँ, लोकक्षयकृत् लोकों का विनाश करने वाला, प्रवृद्धः बड़ा हुआ, लोकान् लोकों को, समाहर्तुम् - नष्ट करने के लिए, अहँ -यहां, प्रवृत्तः लगा हूँ, ऋते-बिना, अपि भी, त्वाम् - तुम्हारे, न नहीं, भविष्यन्ति होंगे (रहेंगे), सर्वे सब, येथे, अवस्थिताः-स्थित, प्रत्यनीकेषु विपक्षी सेना में, योधाः योद्धा ।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : लोकों का विनाश करने वाला इस समय में बड़ा हुआ महाकाल हूँ और लोकों को नष्ट करने में प्रवृत्त हूँ। विपक्षी सेना में स्थित सब योद्धा तेरे बिना भी नहीं रहेंगे।
व्याख्या : ऋतेऽपि त्वाम् - हे अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी मेरे द्वारा इनका अन्त निश्चित ही है। मैं सर्वनाशकारी काल हूँ। मैं पहले से ही उन्हें मार चुका हूँ। तुमने उन्हें मृत्यु के मुख में जाते देखा है। इसलिए तुम्हारा इनको मारने का साधन बनना विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है।
अतः, उठो और यश प्राप्त करो।
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व
जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् ।
मयैवैते निहताः पूर्वमेव
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ।। ३३ ।।
शब्दार्थ : तस्मात् - अतः, त्वम्-तुम, उत्तिष्ठ उठो, यशः यश, लभस्व-प्राप्त करो, जित्वा-जीत कर, शत्रून्-शत्रुओं को, भुङ्क्ष्व-भोग करो, राज्यम्-राज्य, समृद्धम् समृद्ध, मया मेरे द्वारा, एव-ही, एते-ये, राज्या-मारे जा चुके हैं, पूर्वम् -पहले से ही, एव-ही, निमित्तमात्रम् -निमित्त (साधन) मात्र, भव-बनो, सव्यसाचिन् - हे सव्यसाची ।
अनुवाद : इसलिए, उठो और यश प्राप्त करो। शत्रु को जीत कर अप्रतिम राज्य का उपभोग करो। हे अर्जुन, निश्चित रूप से वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं तुम केवल निमित्त बनो।
व्याख्या : तुम केवल नाम मात्र के कारण बनो। मैंने तो पूर्वतः ही उनका विनाश कर दिया है। बहुत पहले ही मैं उन्हें नष्ट कर चुका हूँ।
यश:-लोग सोचेंगे कि भीष्म, द्रोण तथा अन्य योद्धा जिनको देवता भी नहीं मार सकते, वे तुम्हारे द्वारा पराजय को प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार तुम्हारा कीर्ति-ध्वज ऊँचा फहरायेगा। धार्मिक कृत्यों के कारण ही ऐसा यश प्राप्त होगा ।
शत्रून् दुर्योधन जैसे शत्रु ।
सव्यसाची-अर्जुन, जो वाम हस्त से भी बाण चलाने में कुशल था।
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णं तथाऽन्यानपि योधवीरान् ।
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ।।३४ ।।
शब्दार्थ : द्रोणम् द्रोण, च-और, भीष्मम् - भीष्म, च-और, जयद्रथम् जयद्रथ, च-और, कर्णम् -कर्ण, तथा-और, अन्यान् अन्य, अपि-भी, योधवीरान् वीर योद्धा, मया-मेरे द्वारा, हतान्मारे गये, त्वम् - तुम, जहि-मारो, मा-नहीं, व्यथिष्ठाः - विचलित होओ, युध्यस्व-युद्ध करो, जेतासि-जीतोगे, रणे-रण में, सपत्नान्-शत्रुओं को ।
अनुवाद : द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और अन्य शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अब तुम भय से विचलित न हो कर इन्हें मारो। युद्ध करो, तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे।
व्याख्या : मया हतान् - मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके योद्धाओं को मार कर, हे अर्जुन, तुम पाप के भागी नहीं बनोगे ।
द्रोण के पास दिव्य शस्त्र थे। धनुर्विद्या में वे अर्जुन के गुरु थे। वे अर्जुन के अत्यधिक प्रिय और महानतम गुरु थे। भीष्म के पास भी दिव्य शस्त्र थे। उन्हें इच्छा-मृत्यु का वरदान था। वे एक बार अकेले परशुराम से लड़े और विजयी हुए। वे इतने शक्तिशाली थे।
जयद्रथ के पिता ने एक संकल्प ले कर तपश्चर्या की- "जो व्यक्ति मेरे पुत्र के सिर को धरती पर गिराने का कारण बनेगा, वह स्वयं भी गिर जायेगा अर्थात् मृत्यु को प्राप्त होगा।" युद्ध के समय में, अर्जुन के बाण से जयद्रथ का सिर कटा और उसके पिता की गोद में जा गिरा और उन्होंने अनवधान वश उसे धरा पर गिरा दिया और स्वयं भी उसी क्षण मृत्यु की गोद में सो गये। सूर्य पुत्र कर्ण ने इन्द्र से एक अमोघ अस्त्र प्राप्त किया था।
सञ्जय उवाच
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं
सगढ़दं भीतभीतः प्रणम्य ।। ३५ ।।
शब्दार्थ : एतत् वह, श्रुत्वा सुन कर, केशवस्य केशव के, कृताञ्जलिः करबद्ध, किरीटी-अर्जुन, नमस्कृत्वा नमस्कार कर के, आह-कहा, कृष्णम् -कृष्ण को, सगद्रदम्-रुँघे हुए काँपते हुए, प्रणम्य-प्रणाम कर के। वेपमानः-काँपते हुए, भूयः पुनः, एव-ही, कंठ से, भीतभीतः - भय से वचनम् वचन,
सञ्जय ने कहा
अनुवाद : भगवान् कृष्ण के उन वचनों को सुनकर अर्जुन ने काँपते हुए करबद्ध हो कर भगवान् को प्रणाम किया और पुनः भय से काँपते हुए नमस्कार कर के रुँधे हुए कण्ठ से, कृष्ण से कहा-
व्याख्या : अत्यधिक भय अथवा उल्लास की अवस्था में व्यक्ति भावों की वेदना अथवा हर्षोल्लास में आँसू बहाता है। ऐसी अवस्था में उसका कण्ठ रुँध जाता है और वाक् लड़खड़ाने लगती है अथवा वह अस्पष्ट उच्चारण करता है अथवा सँधे गले से बोलता है। अर्जुन भगवान् का विश्वरूप दर्शन कर के अत्यन्त भयभीत हो गया था अतः गद्गद वाणी (अस्फुट स्वर) से बोला ।
सञ्जय के शब्दों में अर्थवत्ता निहित है। उसने सोचा था कि धृतराष्ट्र पाण्डवों के साथ सन्धि कर लेगा क्योंकि अब उसे ज्ञात हो गया था कि अर्जुन द्वारा कर्ण और द्रोण के मारे जाने पर उपयुक्त सहायता के अभाव में उसके पुत्र निश्चित रूप से मारे जायेंगे। सञ्जय को आशा थी कि परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में शान्ति और हर्षोल्लास का वातावरण बन जायेगा। किन्तु धृतराष्ट्र हठी था। नियति वश उसने इस सुझाव की ओर ध्यान नहीं दिया।
अर्जुन उवाच
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ।। ३६ ।।
शब्दार्थ : स्थाने उपयुक्त है, हृषीकेश- हे कृष्ण, तव-आपकी, प्रकीर्त्या गुणगान करने से, जगत् - विश्व, प्रहृष्यति-आनन्दित होता है, अनुरज्यते-अनुरक्त होता है, च- और, रक्षांसि-राक्षस, भीतानि-डर कर, दिशः-दिशाओं को, द्रवन्ति-भाग रहे हैं, सर्वे-सब, नमस्यन्ति-प्रणाम करते हैं (आपको), च-और, सिद्धसङ्घाः - सिद्ध पुरुष ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे कृष्ण, यह उपयुक्त ही है कि विश्व आपके यश का गुणगान करने में आनन्द और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। राक्षस आपके भय से सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध पुरुष आपको प्रणाम कर रहे हैं।
व्याख्या : प्रकीर्त्या -भगवान् की महिमा का गुणगान
भगवान् ही प्रशंसा, प्रेम और प्रसन्नता के पात्र हैं क्योंकि वे सबके मित्र और आत्म-तत्त्व हैं।
भगवान् प्रशंसा, प्रेम और प्रसन्नता के विषय इसलिए भी हैं क्योंकि वे ब्रह्मा के भी स्रोत हैं जो सृष्टिकर्ता हैं।
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे।
अनन्त देवेश जगन्निवास
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ।। ३७ ।।
शब्दार्थ : कस्मात् -किसलिए (क्यों), चऔर, ते-वे, न-नहीं, नमेरन् -प्रणाम करें, महात्मन् -हे महात्मन्, गरीयसे- श्रेष्ठतर, ब्रह्मण:- ब्रह्मा से अपि भी, आदिकरें मूल कारण, अनन्त-अनन्त पुरुष, देवेश देवों के स्वामी, जगन्निवास-जगत् के आश्रय, त्वम्-आपअक्षरम्-अक्षर, सत् सतु, असत्-असत्, तत्वह, परम् परम, यत् -जो ।
अनुवाद : हे महात्मन्, वे आपको नमस्कार क्यों न करें आप जो आदि सृष्टा ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतर हैं। हे अनन्त, हे देवेश, हे जगदाधार, आप अविनाशी हैं, सत् (अस्तित्वमान्) हैं, असत् (अनस्तित्वमान्) हैं और उससे भी अतीत हैं।
व्याख्या : भगवान् महात्मा हैं। वे अन्य सब से बड़े हैं। अविनाशी हैं। इसलिए वे आराधना, प्रेम और हर्ष के समुचित विषय हैं।
तीनों कालों में जो अस्तित्वमान् है वह सत् है। ब्रह्म सत् है। जो तीनों कालों में नहीं है वह असत् है। यह जगत् असत् है। यह शरीर असत् है।
सत् और असत् शब्दों का अभिप्राय अव्यक्त और व्यक्त भी है जो अक्षर ब्रह्म की उपधियाँ हैं। वस्तुतः अक्षर इन दोनों से परे है। गीता में अक्षर शब्द का प्रयोग कभी तो अव्यक्त (प्रकृति) के लिए प्रयोग में आता है और कभी परब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है।
अनन्त वह है जो तीन सीमाओं देश-काल-वस्तु परिच्छेद से अतीत है। इसकी व्याख्या अ. ११ श्लोक ११ में हो चुकी है।
अर्जुन पुनः भगवान् की इस प्रकार स्तुति करता है-
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।। ३८ ।।
शब्दार्थ : त्वम् - आप, आदिदेवः आदि देव, पुरुषः पुरुष, पुराणः सनातन, त्वम् - 3pi*r * 4 अस्य-इस, विश्वस्य-विश्व के, परम् परम, विधानम्-आश्रय, वेत्ता जानने वाले, असि हो, -जानने योग्य, परम् परम, च और, धाम-धाम, त्वया - आपके द्वारा, -व्याप्त, विश्वम् -विश्व, अनन्तरूप है अनन्त रूपों वालेपुरूष ।
अनुवाद : हे अनन्त रूप भगवन्, आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, जगत् के परम आश्रय हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और परम निधान हैं। आपके द्वारा ही सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है, परिपूर्ण है।
व्याख्या : आदि देवः क्योंकि भगवान् सृष्टि कर्ता हैं।
पुरुषः-क्योंकि भगवान् देह रूप पुरी में वास करते हैं (पुरि शयनात्) ।
निधानम्- महाप्रलय काल में जिसमें जगत् विश्राम लेता है। जैसे पात्र मिट्टी से बनता और मिट्टी में ही लीन होता है। इसी भाँति संसार ब्रह्म से उत्पन्न हो कर उसी में विलीन होता है। अतः ब्रह्म जगत् के उपादान कारण हैं। अतः वे आदि देव और परम निधान (आश्रय) हैं।
वेत्ता-जानने योग्य वस्तुओं को जानने वाला। भगवान् सर्वज्ञ हैं। वे समस्त लोकज्ञाता हैं और इसके निमित्त कारण हैं।
परम धाम-विष्णु का परम धाम । रज्जु में सर्प की भाँति ब्रह्म अथवा विष्णु अपनी सत्-चित्-आनन्द पूर्ण प्रकृति से सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हैं।
और भी-
वायुर्यमो ऽग्निर्वरुणः शशांकः
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।।३९ ।।
शब्दार्थ : वायुः वायु, यमः-यम, अग्निः-अग्नि, वरुणः वरुण, शशांकः- चन्द्र, प्रजापतिः-प्रजापति, त्वम् - आप, प्रपितामहः-सब का पितामह, च और, नमः नमः बारम्बार नमस्कार, ते-आपको, अस्तु-हो, सहस्रकृत्वः- हजारों बार, पुनःपुनः, च-और, भूयः पुनः, अपि-भी, नमः नमः नमस्कार, ते आपको ।
अनुवाद : आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह (ब्रह्मा के भी पिता) हो। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार । पुनः-पुनः आपको नमस्कार, नमस्कार।
व्याख्या : प्रजापति-मरीचि तथा अन्य सात, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। मरीचि से कश्यप हुए और कश्यप से अन्य सन्तान हुई। इसलिए मरीचि, कश्यप और अन्य, प्रजापति (प्रजा के स्वामी) अथवा प्रजा के देव माने जाते हैं। कुछ लोग कश्यप तथा अन्य प्रजापतियों के भाव में इस शब्द को लेते हैं किन्तु यहाँ क्योंकि प्रजापति शब्द एकवचन में है अतः ब्रह्मा को ही प्रजापति के भाव में लेना समुचित होगा। ब्रह्मा कश्यप के पितामह हैं। ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म हैं। ईश्वर कारण ब्रह्म है जो ब्रह्मा का कारण है। अतः ईश्वर प्रपितामह है। वह ब्रह्मा के भी पिता हैं।
माया ईश्वर की मर्यादित उपाधि है। माया उसका कारण शरीर है। ईश्वर का कोई धाम नहीं है। माया अव्यतिरेक (अभिन्न) अवस्था में है। वह ऐसी अवस्था में है जहाँ प्रकृति के गुण साम्यावस्था में होते हैं। ईश्वर की इच्छा से जब (तीन गुणों की) समता भङ्ग होती है तो तीन गुण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं।
आप चन्द्रमा हैं, इसमें सूर्य भी उद्दिष्ट है।
पुनः, भूयः पुनः पुनः। नमस्कार सहस्रों बार और पुनः नमस्कार। यहाँ इस भाव को दर्शाया गया है कि अर्जुन के मन में भगवान् कृष्ण के प्रति अनन्य, अपार भक्ति और प्रगाढ़ निष्ठा थी। सहस्र बार नमस्कार करके भी उसे सन्तुष्टि नहीं हो रही थी।
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व।
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ।।४० ।।
शब्दार्थ : नमः -प्रणाम, पुरस्तात् -सामने से, अथ-भी, पृष्ठतः-पीछे से, ते-आपको, नमः-प्रणाम, अस्तु-हो, ते-आपको, सर्वतः सब ओर से, एव-ही, सर्व सब, अनन्तवीर्य-असीम शक्ति युक्त, अमितविक्रमः- अपरिमित पराक्रम स्वरूप, त्वम् - आप, सर्वम् -सर्वस्व, समाप्नोषि-सब में रमे हुए, ततः- इसलिए, असि-हो, सर्वः सर्वस्व ।
अनुवाद : आपको प्रणाम हो, आगे से भी और पीछे से भी। सब ओर से आपको प्रणाम हो। हे सर्वात्मन्, आप अनन्त वीर्य, बल और पराक्रम से युक्त हैं, आप सर्वव्यापक हैं अतः आप ही सर्वस्व हैं।
व्याख्या : नमः पुरस्तादथ पृष्ठतः... "मैं आपके समक्ष प्रणाम करता हूँ, पीछे से भी और सब ओर से प्रणाम करता हूँ", ये शब्द भगवान् की सर्वव्याप्त प्रकृति की ओर संकेत करते हैं। सर्वव्यापक आत्मा का आगे और पीछे कैसे हो सकता है? केवल मर्त्य विषयों का ही पुरस्तात् और पृष्ठ भाग सम्भव है, अर्जुन ने ऐसा ही विचार कर के, कि भगवान् का आगे और पृष्ठ भाग है, भगवान् को प्रणाम किया। इसके अतिरिक्त अर्जुन उस समय नितान्त श्रद्धा और भक्ति भाव से पूर्ण था।
हे सर्वः- आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा सर्वव्यापक होने से वह सर्वस्व है सर्वात्मन् है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं।
सर्वतः आप सब दिशाओं में विराजमान् हैं अतः सब ओर हैं। कोई शक्तिशाली तो हो सकता है किन्तु आवश्यक नहीं कि उसमें शत्रु संहार का साहस हो। अथवा वह अल्प शक्ति से सम्पन्न हो सकता है किन्तु भगवान् तो शक्ति और पराक्रम में अनन्त हैं।
आप स्व-आत्म तत्त्व से सर्वत्र व्याप्त हैं।
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
अजानता महिमानं तवेदं
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ।।४१ ।।
शब्दार्थ : सखा-मित्र, इति-इस प्रकार, मत्वा मान कर, प्रसभम् -हठपूर्वक, यत्-जो, उक्तम् -कहा, हे कृष्ण-हे कृष्ण, हे यादव-हे यादव, हे सखा हे मित्र, इति-इस प्रकार, अजानता न जानते हुए, महिमानम् -महिमा को, तव-आपकी, इदम्-इस, मया-मेरे द्वारा, प्रमादात् -प्रमादवश, प्रणयेन-प्रेमवश, वा-अथवा, अपि-भी ।
अनुवाद: आपकी महिमा से अनभिज्ञ, आपको सखा मानते हुए मैंन प्रणयवश अथवा प्रमादवश आपको हे कृष्ण, यादव, हे सखा कह कर सम्बोधन करने की जो धृष्टता की,
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहारशय्यासनभोजनेषु ।
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ।।४२ ।।
शब्दार्थ : यत्-जो, च-और, अवहासार्थम् -विनोद के लिए, असत्कृतः अपमानित किये गये, असि - हो, विहारशय्यासनभोजनेषु-विहार, शब्या, आसन और भोजन के समय में, एकः एक, अथवा अथवा, अपि-मी, अच्युत-हे कृष्ण, तत् - वह, समक्षम् -समक्ष, तत्-वह, क्षामये क्षमा करें, त्वाम्-आपको, अहम् -मैं, अप्रमेयम् अपरिमित ।
अनुवाद : हे कृष्ण, किसी भी प्रकार से, विनोद के लिए खेल-खेल में, शय्या पर लेटे हुए, बैठे हुए अथवा भोजन के समय, अकेले में अथवा सब के समक्ष मैंने आपका उपहास किया हो तो हे अच्युत, उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। हे अप्रमेय, मुझे क्षमा करना ।
व्याख्या : भगवान् का विश्व रूप दर्शन कर के अर्जुन अपने पूर्व परिचित व्यवहार हेतु क्षमा याचना करता है। वह कहता है-"मैं मूर्ख ही बना रहा हूँ। आपकी महानता से अनभिज्ञ, आपके साथ मैंने लौकिक रीति से व्यवहार किया है। मिथ्या मतिवश (भ्रमवश) मैंने आपको अपना सखा माना । मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। आप इस ब्रह्माण्ड के स्रष्टा हो पुनरपि मैंने आपके साथ उपहास किया। मैंने आपसे अवांछित स्वतन्त्रता ली । कृपया क्षमा करें भगवन्।" तत्-वे सब अपराध ।
अच्युत-वह, जो अपरिवर्तनशील है।
तत्समक्षम् - दूसरों के समक्ष ।
अप्रमेयम् - अपरिमित । जिसका तेज और गौरव अपरिमित हैं।
पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ।।४३ ।।
शब्दार्थ : पिता-पिता, असि-हो, लोकस्य-विश्व के, चराचरस्य- बराचर जगत् के, त्वम् आप, अस्य-इसके, पूज्यः पूजा के योग्य, च और, गुरुः गुरु, गरीयान् अत्यन्त पूजार्ह, न नहीं, त्वत्समः आपके समान, अस्ति-है, अभ्यधिकः बढ़ कर, कुतः-कहाँ से, अन्यः-अन्य, लोकत्रये तीनों लोकों में, अपि-भी, अप्रतिमप्रभाव-अनुपम महिमा वाले।
अनुवाद : आप इस चराचर जगत् के पिता हैं। आप ही इस विश्व के आराध्य देव और महान् गुरु हैं। (क्योंकि) आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं, फिर हे अनुपम महिमा वाले भगवन्, आपसे अधिक (श्रेष्ठतर) कोई कैसे हो सकता है ?
व्याख्या : न त्वत्समोऽस्ति-दो अथवा अधिक ईश्वर तो नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता तो विश्व जिस प्रकार से अब चल रहा है वैसे न होता । सभी ईश्वर एक समान मन वाले तो हो नहीं सकते। वे सब पृथक् पृथक् विचार धारा वाले होते। यदि एक सृष्टि की रचना का इच्छुक होता तो दूसरा नष्ट करने की इच्छा रखता ।
जब आपके समकक्ष ही कोई नहीं तो आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है?
पिता-सृष्टिकर्ता । क्योंकि भगवान् सृष्टिकर्ता हैं इसलिए वे पूज्य हैं। बे सर्वोच्च गुरु भी हैं। इसलिए भगवान् अनुपम हैं उनके समान अन्य कोई नहीं।
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ।।४४ ।।
शब्दार्थ : तस्मात् - इसलिए, प्रणम्य-प्रणाम करके, प्रणिधाय-झुका कर, कायम् -शरीर को, प्रसादये-प्रसन्न करने के लिए (क्षमा याचना के लिए), त्वाम् - आपको, अहम् -मैं, ईशम् - भगवान् को, ईड्यम् -पूज्य, पिता-पिता, इव-भांति, पुत्रस्य-पुत्र का, सखा मित्र, इव मित्र का प्रियः-प्रिय, प्रियाया:-प्रिया का, अर्हसि योग्य हैं, सोढुम्-सहन करने के लिए।
अनुवाद : अतः हे पूर्जाह भगवन्, प्रणाम कर के, दण्डवत् (साष्टाङ्ग) प्रणत हो कर मैं आप से क्षमा याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता पुत्र को, मित्र मित्र को और प्रिय अपनी प्रियतमा को क्षमा कर देते हैं उसी प्रकार आप भी मेरे अपराध को सहन करो, क्षमा करो।
व्याख्या : हे भगवन्, जैसे माता अपने शिशु को गोद में ले लेती है आप भी मुझे अपने सीने से लगा लो। मैंने जो कुछ किया और कहा है उसे क्षमा कर दीजिए। मेरे अपराध क्षमा कीजिए। पूर्वकृत् मेरे दोषों की उपेक्षा कीजिए। अज्ञानवश ही मैंने वह सब किया। मैं आपको समर्पित हूँ और क्षमाप्रार्थी हूँ।
अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।
तदेव मे दर्शय देव रूपं
प्रसीद देवेश जगन्निवास ।।४५ ।।
शब्दार्थ : अदृष्टपूर्वम् - पहले न देखा हुआ, हृषितः - प्रसन्न हूँ, अस्मि-हूँ, दृष्ट्वा देख कर, भयेन-भय से, च-और, प्रव्यथितम् -दुःखी है, मनः मन, मे-मेरा, तत्-वह, एव-ही, मे-मुझे, दर्शय-दिखाओ, देव-हे देव, रूपम् -रूप, प्रसीद-दया करो, देवेश- हे देवाधिदेव, जगन्निवास-जगत् के आश्रय।
अनुवाद : जो पहले कभी नहीं देखा, उसे देख कर मैं आनन्दित हूँ किन्तु मेरा हृदय भय से व्याकुल है। हे भगवन्, हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझ पर कृपा करो, आप प्रसन्न हों और अपना पूर्व रूप ही मुझे (पुनः) दिखाओ।
व्याख्या : सामान्य व्यक्ति के लिए विश्व रूप-दर्शन भयावह और अचम्भे में डालने वाला हो सकता है किन्तु एक योगी के लिए यह उत्साहवर्धक, शक्तिवर्धक और आत्मा को प्रेरित करने वाला है।
अर्जुन कहता है- "विश्व रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे तो केवल वही स्वरूप दिखाओ जो मेरे मित्र रूप में था।”
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त -
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ।।४६ ।।
शब्दार्थ : किरीटिनम् -मुकुट पहने हुए, गदिनम् गदा धारण किये हुए, बनहस्तम् -हाथ में चक्र धारण किये हुए, इच्छामि इच्छा करता हूँ, बाम-आपको, द्रष्टुम् देखने की, अहम् मैं, तथैव-वैसे ही, तेनैव वहीं, रूपण रूप से, चतुर्भुजेन चतुर्भुज रूप से, सहस्रबाहो-हे सहस्रबाहो, भव-हो, विश्वमूर्ते-हे विश्वरूप ।
अनुवाद : हे विश्व रूप, हे सहस्रबाहो, मैं आपको उसी चतुर्भुज रूप में, मुकुट धारण किये हुए, हाथों में चक्र और गदा लिए हुए (पूर्व रूप में) देखना चाहता हूँ।
व्याख्या : अर्जुन ने कहा- "हे भगवन्, विश्वरूप में मैं नहीं जानता मैं किसको सम्बोधन करूँ और किधर, किसके सम्मुख होऊँ। मैं भय से व्याकुल हूँ। मैं आपको शंख, चक्र, गदा, पद्य युक्त देखने का इच्छुक हूँ। इस विश्व रूप को हटा कर पूर्व चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए।"
आध्यात्मिक साधक प्रायः साधना प्रारम्भ करते ही सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों की आकांक्षा करते हैं। यह उचित नहीं है। वे उस तेज पुंज अथवा शक्ति को सहन नहीं कर पायेंगे अतः धैर्य धारण करें।
सहस्रबाहो- विश्व रूप को परिलक्षित करता है।
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ।।४७ ।।
शब्दार्थ : मया-मेरे द्वारा, प्रसन्नेन-प्रसन्न, तव-तुम्हें, अर्जुन-हे अर्जुन, इदम् - यह, रूपम् रूप, परम् -परम, दर्शितम्-दिखाया गया, आत्मयोगात् - अपनी ही योग शक्ति से, तेजोमयम्, रोज युक्त, विधम्-वैषिक, आत्मयोगात अनन्त, आद्यम् - आदि, यत् जो देखो गयेरा, त्वत्-तुम से, अन्येन-अन्य के द्वारा, न-नहीं, दृष्टपूर्वम् -पहले देखा गया।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : हे अर्जुन, यह तेजोमय, अव्युत्पन्न (आदि), अनन्त स्वरूप तुम से प्रसन्न हो कर अपनी दिव्य योग शक्ति से मैंने तुम्हें दिखाया है। यह विराद स्वरूप तुम से पूर्व किसी और ने नहीं देखा ।
व्याख्या : भगवान् कृष्ण विराट् स्वरूप की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसने सार्वभौमिक स्वरूप के दर्शन करके सर्वस्व प्राप्त कर लिया है।
उत्कृष्ट दर्शन प्राप्ति हेतु अभीप्सा रखने के लिए समस्त आध्यात्मिक साधकों के लिए यह प्रेरणा भी है। उन्हें क्या करना अपेक्षित है इस विषय में भगवान् श्लोक ५३ से ५५ में उपदेश देते हैं।
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै -
र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।।४८ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, वेदयज्ञाध्ययनै:-यज्ञ और वेदों के अध्ययन द्वारा, न-नहीं, दानैः दान के द्वारा, न-नहीं, च-और, क्रियाभिः- अनुष्ठानों के द्वारा, न-नहीं, तपोभिः - तपश्चर्या द्वारा, उग्रै:- घोर, एवंरूप:- ऐसा रूप, शक्य:- सम्भव, अहम् -मैं, नृलोके-भूलोक में, द्रष्टुम् - देखने के लिए, त्वत्-तुम से, अन्येन-अन्य के द्वारा, कुरुप्रवीर- हे कौरवों में श्रेष्ठ।
अनुवाद : हे कुरुप्रवीर (अर्जुन), इस मनुष्य लोक में, मेरा यह स्वरूप तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा, न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न कर्मकांड की क्रियाओं से और न ही कठोर तप से देखा जा सकता है।
व्याख्या : बिना अर्थज्ञान के वेदों को मात्र कण्ठस्थ कर लेने से ज्ञान नहीं होता । क्रियाओं का अध्ययन और उनका अर्थ जानना भी अनिवार्य है। दान-जैसे तुला पुरुष अर्थात् मनुष्य के भार के अनुरूप स्वर्णदान ।
कन्यादान-अपनी गोदान, अन्नदान आदि हैं। पुत्री को विवाह के समय दान करना। इसी प्रकार
क्रिया-अग्निहोत्र आदि क्रियायें।
तपस् -जैसे चान्द्रायण व्रत-इसमें पूर्णिमा से प्रारम्भ कर के कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक-एक ग्रास कम करते जाते हैं और इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में नित्य एक-एक ग्रास बढ़ाते जाते हैं। यह व्रत मन की शुद्धि करने वाला और पापनाशक है।
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् ।
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।।४९ ।।
शब्दार्थ : मा-मत (नहीं), ते तुम, व्यथा-डरो, मा-नहीं, चऔर, विमूढभावः किंकर्तव्यविमूढ़ होना, दृष्ट्वा-देख कर, रूपम् रूप, घोरम् - विकराल, ईदृक् -ऐसे, मम-मेरे, इदम् -इस, व्यपेतभीः- भय रहित हो कर, प्रीतमनाः - प्रसन्न मन से, पुनः पुनः, त्वम्-तुम, तत्-उस, एव-ही, मे-मेरे, रूपम् -रूप को, इदम् - यह, प्रपश्य-देखो ।
अनुवाद : मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देख कर भयभीत न होओ और न ही किंकर्तव्यविमूढ़ बनो। भय को त्याग कर प्रसन्न चित्त से पुनः मेरे पूर्व स्वरूप को देखो ।
व्याख्या : पूर्व रूप-शंख, चक्र, गदा, पद्य युक्त पूर्व रूप अर्थात् चतुर्भुज रूप ।
भगवान् ने अर्जुन को भयभीत दशा में देखा, इसलिए उन्होंने अपना विश्वरूप परिवर्तित कर के पूर्व सौम्य रूप धारण किया। अर्जुन को सान्त्वना देते हुए वे प्रेमपूर्ण मधुर वचन बोले ।
सञ्जय उवाच
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।
आश्वासयामास च भीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ।।५० ।।
शब्दार्थ: इति-इस प्रकार, अर्जुनम् अर्जुन को, वासुदेवः वासुदेव, तथा-पैसा, उक्त्वा कह कर, स्वकम् - अपने, रूपम् -रूप को, दर्शयामास जैसा उसुना, आश्वासयामास - आश्वासन दिया, चऔर, भीतम् डरे दिवा एनम् उसे, भूत्वा हो कर, पुनः पुनः, सौम्यवपुः सौम्य स्वरूप, महात्मा-महात्मा ।
सञ्जय ने कहा
अनुवाद : अर्जुन को इस प्रकार कह कर भगवान् कृष्ण ने पुनः अपना स्वरूप दिखाया और (इस प्रकार) महात्मा (कृष्ण) ने सौम्य स्वरूप धारण कर के भयभीत अर्जुन को आश्वासित किया ।
व्याख्या : मे रूपमिदम् - वसुदेव के पुत्र के रूप में।
अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ।।५१ ।।
शब्दार्थ : दृष्ट्वा देख कर, इदम्-यह, मानुषम् - मनुष्य का, रूपम् -रूप, तव-आप का, सौम्यम्-सौम्य, जनार्दन हे कृष्ण, इदानीम् - अब, अस्मि-हूँ, संवृत्तः स्थिर, सचेताः- चेतना युक्त (अपनी चेतना में), प्रकृतिम् - प्रकृति को, गतः- प्राप्त ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे कृष्ण, आपके इस सौम्य मानव स्वरूप को देख कर मेरा चित्त स्थिर हो गया है और मैं अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया हूँ।
व्याख्या : अर्जुन भगवान् कृष्ण से कह रहे हैं-"हे भगवन्, अब मैं आपको मनुष्य रूप में देख रहा हूँ। अब मेरे विचार संहृत हो गये हैं और मैं शान्त हो गया हूँ। मैं बोल सकता हूँ। मेरी इन्द्रियाँ अपना कार्य कर रही हैं। मैं भय मुक्त हो गया हूँ। भूल करने वाले शिशु को भी जिस प्रकार माता गोद में ले कर कण्ठ से लगा लेती है, आपने वैसा ही प्यार मुझे दिया है, मेरे साथ मातृवत् व्यवहार किया है। कुछ दिन तक माँ से बिछुड़ा हुआ गोवत्स (बछड़ा) जिस प्रकार माँ को पुनः देख कर हर्षित होता है उसी प्रकार आपके इस अत्यन्त सुन्दर स्वरूप को देख कर मैं आनन्द की अनुभूति कर रहा हूँ। मैंने अमृतपान कर लिया है, अब मैं जीवित हूँ।”
श्री भगवानुवाच
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ।।५२ ।।
शब्दार्थ : सुदुर्दर्शमिदम् -दुर्लभ दर्शन वाला, इदम् - यह, रूपम् -रूप, दृष्टवानसि तुमने देखा है, यत्-जो, मम-मेरा, देवा -देव, अपि - भी, अस्य -इस, रूपस्य रूप के, नित्यम् - नित्य, दर्शनकाङ्क्षिणः - दर्शन के ।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : मेरा जो स्वरूप तुमने देखा है इसे देख पाना वस्तुतः अत्यन्त कठिन है। देवगण भी इस रूप के दर्शन के लिए नित्य आकाङ्क्षा करते हैं।
व्याख्या : भगवान् कृष्ण अर्जुन से कहते हैं- "यद्यपि देवगण इस विश्वरूप दर्शन की अभिलाषा रखते हैं तथापि उन्हें दर्शन नहीं हुए, जैसे तुम्हें हो गये। वे इसे कभी नहीं देख सकते।"
उत्सुकतापूर्वक मेघों को देखते हुए जिस प्रकार चातक पक्षी वर्षा की एक बूँद की कामना करता है उसी प्रकार देवगण विश्व रूप दर्शन के लिए स्पृहा करते हैं किन्तु स्वप्न में भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है। ऐसा अद्भुत है यह विश्व रूप दर्शन जिसे तुमने सहज ही पा लिया है।
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ।।५३ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, अहम् -मैं, वेदैः- वेदों के द्वारा, तपसा तपस्या के द्वारा, न नहीं, दानेन दान के द्वारा, न-नहीं, च-और, इज्यया-यज्ञ से, शक्यः-सम्भव, एवंविधः - इस प्रकार, द्रष्टुम् - देखने के लिए, दृष्टवानसि - (तुमने) देखा है, माम् -मुझे, यथा-जैसे ।
अनुवाद : (इतने सहज रूप से), जैसे तुमने मुझे देखा है ऐसे न तो मैं वेदों से, न तपश्चर्या से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूँ।
व्याख्या : विश्व रूप दर्शन जो तुमने इतनी सुगमतापूर्वक कर लिया है बह न तो वेद और षड्दर्शन के अध्ययन से , न यज्ञादि क्रियाओं से (तपस्या से), न दान से और न ही विविध प्रकार के अनुष्ठान आदि से सुलभ है।
वास्तव में ही अर्जुन अत्यन्त सौभाग्यशाली था कि उसको विराट् रूप के दर्शन सुलभ हुए।
भगवान् के दर्शन कैसे सुलभ हैं? सुनो! हृदय उसकी सच्ची भक्ति से आप्लावित हो जाये, परिपूर्ण हो जाये । (निरूपण-XI.48)
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ।।५४ ।।
शब्दार्थ: भक्त्या-भक्ति से, तु-निश्चयेन, अनन्यया-अनन्य (भक्ति) से, शक्य:- (मैं) सम्भव हूँ, अहम् -मैं, एवंविध:- इस रूप वाला, अर्जुन- हे अर्जुन, ज्ञातुम्-जानने के लिए, द्रष्म् देखने के लिए, च-और, तत्त्वेन-तत्व से, प्रवेष्टुम् -प्रवेश करने के लिए, च-और, परंतप हे अर्जुन ।
अनुवाद : हे अर्जुन, निश्चित रूप से अनन्य भक्ति भाव के द्वारा मेरा यह विराट् स्वरूप तत्त्व से जाना और देखा जा सकता है तथा इसमें प्रवेश पाया जा सकता है अर्थात् इसका गोपनीय रहस्य समझा जा सकता है।
व्याख्या : विश्व रूप दर्शन हेतु केवल भक्ति एकमात्र साधन है।
अनन्य भक्ति-एकाग्र चित्त से भक्ति। एक ही लक्ष्य के भेदन हेतु अनवरत भक्ति । वह भक्ति जिसमें भगवान् के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की अभीप्सा नहीं होती। इस प्रकार की भक्ति में किसी भी इन्द्रिय द्वारा अपने भगवान् के अतिरिक्त अन्य किसी विषय की अनुभूति नहीं होती । अहंभाव और द्वैत भाव पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं।
एवंविधः - इस प्रकार का अर्थात् विराट् स्वरूप का ।
अनन्य भक्ति से न केवल मुझे जानना ही पर्याप्त है, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है प्रत्युत् मेरा साक्षात्कार अथवा मोक्ष भी सम्भव है। भक्त यह जान लेता है कि ये सब भी भगवान् है और आत्यन्तिक सत्य भी वही है। इस प्रकाश की अनुभूति होने पर उसमें (भगवान् में) लीन हो जाता है। (निरूपण-VIII. 22; X.10)
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।।५५ ।।
शब्दार्थ : मत्कर्मकृत् -मेरे लिए कर्म करने वाला, मत्परमः मुझे परम पुरुष मानने वाला, मद्भक्तः- मेरा भक्त, सङ्गवर्जितः- आसक्ति रहित, निर्वैरः- वैर भाव से मुक्त, सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में, यः-जो, सः-वह, माम् -मुझे, एति-प्राप्त होता है, पाण्डव-हे अर्जुन।
अनुवाद : जो मनुष्य मेरे लिए ही सब कर्म करता है, मुझे ही सर्वोच्च सत्ता मानता है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है, किसी भी प्राणी के प्रति वैरभाव नहीं रखता, वह, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होता है।
व्याख्या : सम्पूर्ण गीता का यह सार है। इस उपदेश के अनुरूप अपना जीवन बनाने वाला साधक परम आनन्द और अमृतत्व की प्राप्ति करेगा। गीता के सम्पूर्ण दर्शन का, यह श्लोक सार तत्त्व है।
भगवान् के लिए ही जो साधक कर्त्तव्य कर्म करता है, भगवान् को ही समस्त कर्म समर्पित करता है, हृदय से, आत्मा से उसकी सेवा करता है, उसे अपना परम लक्ष्य मानता है, उसी के लिए ही जीवित रहता है, उसी के लिए कर्म करता है, सब में भगवान् के दर्शन करता है, समस्त संसार को भगवान् का विश्व रूप दर्शन मान कर, दूसरों द्वारा अपमानित होने पर किसी के लिए घृणा अथवा शत्रु भाव नहीं रखता, धन-दौलत में आसक्ति नहीं रखता, सन्तति, पत्नि, मित्र और सम्बन्धियों के प्रति भी आसक्ति से मुक्त रहता है, और भगवान् के अतिरिक्त कोई और आकाङ्क्षा नहीं रखता, वह साक्षात्कार द्वारा उस परम सत् से एकत्व प्राप्त कर लेता है, उसी के साथ एक रूप हो जाता है।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ।।
।। इति विश्वरूपदर्शनयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ द्वादशोऽध्यायः
भक्तियोगः
अर्जुन उवाच
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ।।१ ।।
शब्दार्थ : एवम् - इस प्रकार, सततयुक्ताः सदा स्थिर, ये-जो, भक्ताः- भक्त, त्वाम् - आपको, पर्युपासते- (आपकी) उपासना करते हैं, ये-जो, च-और, अपि-भी, अक्षरम् -अविनाशी, अव्यक्तम् -अव्यक्त, तेषाम् -उनका, के -कौन, योगवित्तमाः -योग में श्रेष्ठ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : वे भक्त जो आपकी ही भक्ति में अनन्यमनस्क हो कर संलग्न हैं और अन्य वे जो अव्यक्त अविनाशी परब्रह्म की उपासना में लगे हैं, इनमें श्रेष्ठतर योगवेत्ता कौन हैं?
व्याख्या : द्वादश अध्याय इस सत्य को प्रमाणित करता है कि ज्ञानयोग की अपेक्षा भक्ति योग अधिक सहज है। भक्ति योग में भक्त भगवान् से प्रिय और सन्निकट का सम्बन्ध स्थापित करता है। वह अपनी सामर्थ्य, रुचि और स्वभाव के अनुरूप पाँच भावों में से किसी एक का चयन करता है। पाँच भाव इस प्रकार हैं-शान्त भाव (शान्तिपूर्वक आराधना), दास्य भाव (सेवक और स्वामी का भाव), सखा भाव (सखा का भाव, भगवान् के प्रति), वात्सल्य भाव (पिता-पुत्र-भाव), माधुर्य भाव (प्रेमी और प्रेमिका का भाव)। भक्त इन भावों को अपने भगवान् के प्रति रखता है। अन्तिम, माधुर्य भाव भक्ति की पराकाष्ठा है। यह भगवान् में लीन होना है। भक्त भगवान् की वन्दना करता है। वह उनका सतत स्मरण करता है। उन का कीर्तन करता है। उनकी महिमा का गुणगान करता है। नाम-जप करता है। उनके मन्त्र का जप करता है। प्रार्थना करता है और साष्टाङ्ग प्रणाम करता है। उनकी लीला का श्रवण करता है। वह इच्छारहित, असूया रहित, बिना किसी शर्त के पूर्ण समर्पण करता है और भगवान् की अहेतुकी अनुकम्पा का अधिकारी बन जाता है, उनसे संलाप करता है और अन्ततः उन्हीं में समा जाता है।
भक्त की उपासना मूर्ति पूजा से प्रारम्भ होती है। इसके उपरान्त वह उस रूप की आन्तरिक (मानसिक) पूजा-आराधना करता है। अन्ततः वह सर्वव्यापक परमात्मा की परम-पूजा में प्रेरित किया जाता है।
एवम् - इस प्रकार अर्थात् जैसा पूर्व अध्याय के अन्तिम श्लोक में कहा गया। अव्यक्तम् अव्यक्त अर्थात् सीमित उपाधियों से अतीत, इन्द्रियों द्वारा अबोधगम्य ।
अव्यक्त ब्रह्म सब सीमाओं से परे है। इन्द्रियों द्वारा जो कुछ दृष्टिगोचर है वह व्यक्त है।
भक्तों के हृदय पूर्णरूपेण आप पर एकाग्रित रहते हैं। वे पूर्ण मन से, आत्मा से आपकी आराधना करते हैं।
अन्य वे हैं जो देश-काल-वस्तु-परिच्छेद से अतीत निर्गुण, निराकार, अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं जो शाश्वत है, अनिर्वचनीय है तथा मन और इन्द्रियों की पहुँच से परे है। ऐसे उपासक ज्ञानी ऋषि होते हैं।
भक्त और ज्ञानी-अब इन दोनों में से श्रेष्ठतर योगवेत्ता कौन है? (निरूपण-XI.55)
श्री भगवानुवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ।।२ ।।
शब्दार्थ : मयि-मुझ में, आवेश्य स्थिर कर के, मन:-मन, ये जो, भाम्-मुझे, नित्ययुक्ताः सतत लगे हुए, उपासते-पूजा करते हैं, भार आबद्धापूर्वक, परया-परम, उपेताः युक्त, से-वे, मे-मेर, युक्ततमाः- योग में उत्कृष्टतम, मताः- (मेरे) विचार में।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : मुझ में मन स्थिर कर के, सतत ध्यान मग्न और परम निष्ठा के साथ जो मेरी उपासना करते हैं, वे योग में उत्तम हैं, ऐसा मेरा मत है।
व्याख्या : जो भक्त अपने मन को मुझ में, मेरे विश्व रूप में स्थिर करते हैं और सदा समन्वित, परम श्रद्धापूर्वक, मुझे सब योगों का स्वामी मानते हुए, अनासक्त भाव से, सब बुराइयों से दूर रह कर मुझ परम पुरुष की आराधना करते हैं वे मेरे विचार से योग में उत्तम हैं।
वे अहोरात्र मेरे भजन में व्यतीत करते हैं। मेरे विचार के अतिरिक्त उनके मन में अन्य कोई विचार नहीं आता। वे मेरे लिए जीवन यापन करते हैं। अतः यह कहना समुचित ही है कि वे उत्तम योगी हैं।
जो अव्यक्त, निर्गुण, निराकार परब्रह्म की उपासना करते हैं, क्या वे उत्तम योगी नहीं हैं? उनके विषय में भी सुनो...
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ।।३ ।।
शब्दार्थ : ये-जो, तु-निश्चित रूप से, अक्षरम् - अविनाशी, अनिर्देश्यम् अनिर्वचनीय, अव्यक्तम्-अव्यक्त की, पर्युपासते-उपासना करते हैं, सर्वत्रगम् सर्वव्यापक, अचिन्त्यम् -चिन्तन से परे, च-और, कूटस्थम् - अपरिवर्तनशील, अचलम् -अचल, ध्रुवम् - शाश्वत ।
अनुवाद : जो अविनाशी, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, अपरिवर्तनशील, अचल और ध्रुव (शाश्वत) की उपासना करते हैं,
व्याख्या : अनिर्देश्यम्-जिसके विषय में न तो कुछ कहा जा सकता है और न ही उसके दर्शन कराये जा सकते हैं वह अक्षर, परब्रह्म सच्चिदानन्द मन और वाणी से परे है अर्थात् मन उसका चिन्तन नहीं कर सकता और वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। वह क्यों नहीं निर्दिष्ट हो सकता, क्योंकि वह अव्यक्त है। व्यक्त प्राणियों के चार लक्षणों का उसमें अभाव है जैसे-जाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि), गुण (श्वेत वर्ण, नील वर्ण, लम्बा, छोटा आदि), क्रिया (पढ़ना, लिखना आदि), और सम्बन्ध (जैसे पिता-पुत्र का सम्बन्ध आदि) ।
अव्यक्त-किसी भी ज्ञानेन्द्रिय द्वारा जो बोधगम्य न हो, किसी ज्ञानेन्द्रिय के समक्ष अभिव्यक्त न हो।
उपासना-समीप बैठना। पूजा के लिए चयन किये गये लक्ष्य (विषय) के समीप बैठना और उस पर ध्यान एकाग्र करना आध्यात्मिक आचार्य के उपदेश एवं शास्त्र विधि के अनुरूप विचार-प्रवाह को तैलधारवत् समाहित कर के एकाग्रता और स्थिरता लाना उपासना है। यह सतत, अबाधित भगवत् ध्यान है।
अविनाशी ब्रह्म सर्वव्याप्त है, आकाशवत् प्रत्येक वस्तु को आच्छादित किये हुए हैं। अव्यक्त होने से यह अचिन्त्य है। इन्द्रियों द्वारा दृष्टिगोचर प्रत्येक वस्तु मन के चिन्तन में आ सकती है। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ग्राह्य ज्ञान मन भी ग्रहण करता है। किन्तु परम पुरुष इन्द्रियों के लिए अदृश्य है अतः ज्ञानेन्द्रियाँ इसको ग्रहण नहीं कर सकतीं और इसी कारण से वह चिन्तन से भी परे है। परमात्मा के समस्त विचार अन्ततोगत्वा साधक को स्थिर, अचल, शान्त, ध्यान की ओर प्रेरित करते हैं।
यह कूटस्थ (अपरिवर्तनशील) है। कूटस्थ का अभिप्राय है एक ढेर के भाँति पड़े रहना । अतः यह अव्यय (निर्विकार) और नित्य है। स्थूणा (जिस पर लुहार अपना कार्य करता है) पर पीटे जाने पर जिस प्रकार लौह खण्ड अपना स्वरूप बदलते हैं किन्तु स्थूणा स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता उसी प्रकार ब्रह्म अपरिवर्तनशील है किन्तु रूप बदल रहे हैं। इसीलिए ब्रह्म को कूटस्थ कहा जाता है। कोई वस्तु जो बाहर से सुन्दर हो किन्तु भीतर से दोषपूर्ण हो, वह भी 'कूट' कहलाती है। इस अभिप्राय से इसका संकेत संसार के बीज अर्थात् 'अज्ञान' की ओर है जो भीतर से दोषयुक्त है और श्वेताश्वतरोपनिषद् में जिसे अव्यकृत कहा गया है (मायां तु प्रकृतिं विद्यात्, मायिनं तु महेश्वरम्) और गीता में (मम माया दुरत्यया-मेरी माया का उच्छेदन अत्यन्त कठिन है-V114) इस प्रकार कहा जाता है। कूटस्थ की एक और व्याख्या है- 'जो प्रत्येक वस्तु का मूल है।' जो माया में कूटस्थ, स्वामी और साक्षी रूप से स्थित है।
अचलम् - स्थिर । अपरिवर्तनशील। अतः अविनाशी ब्रह्म ध्रुव है और शाश्वत है। (निरूपण-VIII.21)
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।।४ ।।
शब्दार्थ : संनियम्य-संयत करके, इन्द्रियग्रामम् इन्द्रियों को, सर्वत्र सर्वत्र, समबुद्धयः समान भाव वाले, ते-वे, प्राप्नुवन्ति-प्राप्त करते हैं, माम् -मुझे, एव-ही, सर्वभूतहिते सब प्राणियों के कल्याण में, रताः- लगे हुए।
अनुवाद : सब इन्द्रियों को वश में कर के समबुद्धि साधक सर्वत्र, प्राणी मात्र के कल्याण में लगे हुए निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होते हैं।
व्याख्या : राग-द्वेष से मुक्त व्यक्ति मन का समत्व प्राप्त कर सकते हैं। आत्म-ज्ञान से जिन्होंने सुख-दुःख के मूल कारण अज्ञान को नष्ट कर लिया है और जिन्होंने विषय-वासनाओं (इन्द्रिय सुख) में दोष दृष्टि रखने का सतत अभ्यास करके ऐन्द्रिक तृष्णाओं के जाल से मुक्ति पा ली है वे समबुद्धि हैं। अभीप्सित अथवा अनभीप्सित वस्तु के प्राप्त होने पर जो न तो हर्षित होते हैं। और न ही दुःखी होते हैं वे समबुद्धि हो सकते हैं।
अनुराग और विद्वेष की दो धारायें मनुष्य को, दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए प्रेरित करती हैं। ध्यानाभ्यास के द्वारा जब इनका विनाश हो जाता है तब योगी लोक कल्याण में निरत होता है। जनगण की सेवा में वह आनन्द लेने लगता है। वह स्वयं को सेवा में व्यस्त कर लेता है। वह अनवरत रूप से संसार के कल्याण के लिए कार्यरत रहता है। वह सब प्राणियों को अभय दान देता है। किसी प्राणी को उससे भय नहीं होता। वह परमहंस संन्यासी बन जाता है जो अपने हृदय में सब को आश्रय प्रदान करता है। वह आत्म-साक्षात्कार द्वारा ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है।
इन्द्रिय-संयम के द्वारा योगी दसों द्वारों को बन्द कर के विषयों से इन्द्रियों का प्रत्याहरण कर के मन को अन्तस्तम आत्मा में स्थिर करता है। इन्द्रिय-संयम और इन्द्रिय-संहरण कर के, लोक-कल्याण में निरत तथा अनश्वर अलौकिक ब्रह्म पर ध्यान करने वाले साधक मुझे ही प्राप्त होते हैं। यह कहना अनिवार्य नहीं है कि वे मेरे पास ही पहुँचते हैं क्योंकि ज्ञानी को मैं अपने से अभिन्न मानता हूँ। (VII. 18.) यह कहना भी आवश्यक नहीं है कि वे उत्तम योगी हैं क्योंकि वे ब्रह्म के साथ एकरूप हैं। ( f 7599-V.25;*1.55)
क्लेशो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ।।५ ।।
शब्दार्थ : क्लेशः दुःख, अधिकतरः-और अधिक, तेषाम् उन, अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, अव्यक्ता-अव्यक्त, हि-क्योंकि, गतिः लक्ष्य, दुःखम्-दुःख, देहवद्भिः- देहधारियों के द्वारा, अवाप्यते-प्राप्त किया जाता है।
अनुवाद : निराकार ब्रह्म (अव्यक्त) में अनुरक्त साधकों की कठिनाई और अधिक है क्योंकि देहधारियों के लिए अव्यक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुगम नहीं है।
व्याख्या : सगुण और निर्गुण ब्रह्म के उपासक एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं किन्तु निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति अत्यन्त यत्नसाध्य और कठिन है क्योंकि साधक के लिए आध्यात्मिक-साधना-काल के प्रारम्भ से ही देहाभिमान का त्याग अनिवार्य होता है। इसी कारण उन्हें और अधिक कष्ट झेलना पड़ता है।
देहवद्भिः देह के साथ एकत्व स्थापित कर लेना देहाभिमान कहा जाता है। अपनी देह से आसक्त अर्थात् देहाभिमानियों के लिए अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त करना दुःसाध्य है। और भी, निराकार, निर्गुण ब्रह्म पर चंचल मन को स्थिर करना भी परिश्रमसाध्य है। अविनाशी, निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान लगाने के लिए कुशाग्र बुद्धि होना भी आवश्यक है। उपनिषद् के अनुसार-"दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभिः", "यह सूक्ष्म द्रष्टा के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से दर्शनीय है।"
अव्यक्त का ध्यान करने वालों के लिए साधना-चतुष्ट्य (III.3) की साधना अभिहित है। तदुपरान्त ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्रनिपुण गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु से सत्य का ज्ञान श्रवण कर के उस पर चिन्तन-मनन और ध्यान करना चाहिए।
निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर शाश्वत शान्ति अथवा कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसके प्रभाव से अज्ञान रूपी अन्धकार का विनाश हो जात ही सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर साधक ब्रह्मलोक को जाता है और भगवान् की शक्तियों और वैभव का आनन्द लेता है। तत्पश्चात् वह हिरण्यगर्भ से परम पुरुष के गोपनीय रहस्यों की दीक्षा लेता है और बिना किसी प्रयास के और बिना श्रवण, मनन और ध्यान के अभ्यास के, भगवत्कृपा से उसी अवस्था को पहुँचता है जो अवस्था निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले साधक ने प्राप्त की थी। सगुण ब्रह्म के उपासकों का भी आत्म-ज्ञान की ज्योति से अज्ञान का अन्धकार और उसके प्रभाव पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।।६ ।।
शब्दार्थ : ये जो, तु किन्तु, सर्वाणि-सब, कर्माणि-कर्म, मयि-मुझमें, संन्यस्य-त्याग कर, मत्पराः- मेरे परायण, अनन्येन-एकाग्र चित्त हो कर, एव-ही, योगेन योग के द्वारा, माम् -मुझे, ध्यायन्तः- ध्यान करते हुए, उपासते-पूजा करते हैं।
अनुवाद : किन्तु वे जो समस्त कर्मों का परित्याग कर के मेरे परायण हो कर (समर्पित भाव से), मुझे परम लक्ष्य मान कर अनन्य योग से ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं।
व्याख्या : अनन्य योग-अचल योग, विलक्षण योग। जिसमें भगवान् के अतिरिक्त अन्य कोई ध्यान का विषय न हो । समाधि की अवस्था । भक्ति योग में भी कर्म अपरिहार्य है। कर्म तो करें किन्तु उसका परिणाम भगवान् को समर्पित करें। (निरूपण-IX.27)
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ।।७ ।।
शब्दार्थ : तेषाम् उनका, अहम् -मैं, समुद्धर्ता-उद्धार करने वाला, मृत्युसंसारसागरात् -मर्त्य संसार रूपी सागर से, भवामि-होता हूँ, नचिरात् शीघ्र ही, पार्थ-हे अर्जुन, मयि-मुझ में, आवेशितचेतसाम् - मुझ में चित्त लगाने वालों का ।
अनुवाद : हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों के लिए मैं अबिरेण ही इस मर्त्यलोक रूप सागर से समुद्धार करने वाला होता हूँ।
व्याख्या : मृत्यु संसार-आवागमन (जन्म-मृत्यु) का चक्र।
वह भक्त जिसने पूर्ण, निरपेक्ष, असूय, आत्म-समर्पण कर दिया है और स्वयं को भगवान् की दया पर पूर्णतया छोड़ दिया है, जो भगवान् पर मन की अनन्यमनस्क भाव से स्थिर करता है, कर्म फल भगवान् को समर्पित कर के उन कमाँ को भस्मीभूत कर लेता है, और कर्म में फल लाने की शक्ति ही नहीं रहने देता और जिसने मोक्ष की लालसा भी त्याग दी है, वह मर्त्य लोक से ऊपर उठ कर भगवान् की शरण, अमर धाम में पहुँचता है। भगवान् स्वयं उसकी सहायता करते हैं।
मच्चित् -मुझ में युक्त मन वाले भक्तों को अविलम्ब मैं इस भौतिक जगत् से मुक्त कर देता हूँ। निरुपण - X .10,, 11; XII.6, 7)
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ।।८ ।।
शब्दार्थ : मयि-मुझ में, एव-ही, मनः- मन, आधत्स्व-एकाग्र करो, मयि-मुझ में, बुद्धिम् बुद्धि को, निवेशय-रखो, निवसिष्यसि -वास करोगे, मयि-मुझ में, एव-ही, अतः ऊर्ध्वम् - इसके पश्चात्, न-नहीं, संशयः-संशय ।
अनुवाद : अपना मन मुझ में ही एकाग्र करो, अपनी बुद्धि भी मुझ में ही स्थिर करो। इसके पश्चात् तुम मुझ में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं ।
व्याख्या : 'मन आधत्स्व' का अभिप्राय है-अपने प्रयोजन और अपने विचार (संकल्प-विकल्प) मुझ में अर्थात् भगवान् के विश्व रूप में स्थिर करो। इन्द्रिय-विषयों को, अन्य सब विचारों को त्याग दो । निश्चयात्मिका बुद्धि को भी मुझ में स्थिर करो।
इसका परिणाम क्या होगा? निस्सन्देह, तुम मुझ में मेरी तरह से वास करोगे। हे अर्जुन, इस विषय में अल्प मात्र भी संशय नहीं है।
इस श्लोक में ध्यान योग का विवरण दिया गया है। (निरूपण-VIII.7; X.9; XI.34; XVIII.65)
अध चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ।।९ ।।
शब्दार्थ : अध-यदि, चित्तम् मन, समाधातुम् -स्थिर करने में, न- नहीं, शक्नोषिसमर्थ हो, मयि मुझ में, स्थिरम् -स्थिरतापूर्वक, अभ्यासयोगेन अनवरत अभ्यास के योग से, ततः-तब, माम् -मेरी, इच्छ-च्छिा करो, आमुम् - प्राप्त करने के लिए, धनञ्जय-हे अर्जुन।
अनुवाद : यदि तुम स्थिरतापूर्वक मुझ में मन लगाने में असमर्थ हो तो हे अर्जुन, अनवरत अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो।
व्याख्या : अभ्यास योग-मन को स्थिर करने और लक्ष्य पर लगाने का निरन्तर अभ्यास, अभ्यास योग है। मन को विषय वासनाओं से हटा कर आत्म-तत्त्व पर अथवा अन्य किसी लक्ष्य पर एकाग्र करना अभ्यास योग है। मायावी पंच कोषों से स्वयं को पृथक् करना और आत्मा से युक्त करना अभ्यास है। यदि तुम अपने मन-बुद्धि को हर समय भगवान् में स्थिर नहीं कर सकते तो किंचित् काल के लिए ऐसा करने का अभ्यास करो। यदि मन अधिक भटकता है तो सतत स्मरण द्वारा इसे संयत करने का प्रयास करो। भगवान् के मूर्त रूप में (मूर्ति आदि में) उसकी विद्यमानता का अनुभव करो। इससे भी सहायता मिलेगी।
यहाँ भगवान् कृष्ण अर्जुन को धनञ्जय क्यों कहते हैं ? कुछ तो महत्त्व होगा? युधिष्ठिर द्वारा किये गये राजसूय यज्ञ के लिए अर्जुन ने बहुत लोगों को विजित कर के अपार धन एकत्र किया। ऐसे महान् तेजस्वी और पराक्रमी पुरुष के लिए मन को जीतना और आत्म-ज्ञान की आध्यात्मिक सम्पदा प्राप्त करना कदापि कठिन नहीं है। इसीलिए यहाँ भगवान् उपदेश देते हुए अर्जुन को 'धनञ्जय' कह कर सम्बोधित करते हैं।
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ।।१० ।।
शब्दार्थ : अभ्यासे-अभ्यास में, अपि-भी, असमर्थ:- असमर्थ, असि-हो, मत्कर्मपरमः- मेरे लिए कर्म परायण, भव-हो जाओ, मदर्थम् - मेरे लिए, अपि-भी, कर्माणि कर्म, कुर्वन् -करते हुए, सिद्धिम् -सिद्धि, अवाप्स्यसि-प्राप्त करोगे।
अनुवाद : यदि तुम यह अभ्यास योग करने में भी असमर्थ हो तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। मेरे निमित्त कर्म करने पर भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे ।
व्याख्या : योग का अभ्यास किये बिना भी यदि तुम मेरे निमित्त ही कर्म करोगे तब भी पूर्णत्व को प्राप्त करोगे। प्रथम तुम मन की शुद्धता प्राप्त करोगे, फिर योग (एकाग्रीकरण और ध्यान), तदुपरान्त ज्ञान और अन्त में मोक्ष प्राप्त करोगे । नारायण भाव से मनुष्य मात्र की सेवा करना अर्थात् सब प्राणियों में नारायण ही हैं, इस भाव से सेवा करने पर भी वह सेवा भगवान् की सेवा मानी जाती है। इस सेवा के साथ-साथ आराधना और ध्यान भी होने चाहिए।
यदि तुम अभ्यास योग नहीं कर सकते (जैसा कि श्लोक ८ में उपदिष्ट है), अथवा सतत अभ्यास भी नहीं कर सकते (श्लोक ९ के अनुसार), तो भगवन्नाम का कीर्तन करो, स्तुति करो और भगवद्भक्तों द्वारा आयोजित धार्मिक प्रवचनों का और महिमान्वित कथाओं का श्रवण करो।
नौ प्रकार के भागवत धर्म का अभ्यास करो- (१) लीला श्रवण, (२) कीर्तन, (३) स्मरण, (४) पादसेवन, (५) अर्चन (पुष्प अर्पित करना), (६) वन्दन (साष्टाङ्ग प्रणाम), (७) दास्य भाव, (८) सखा भाव, (९) आत्म निवेदन (पूर्ण समर्पण)। (निरूपण -III.19; XI.55)
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ।।११ ।।
शब्दार्थ : अथ-यदि, एतत्-यह, अपि-भी, अशक्तः - असमर्थ, असि-हो, कर्तुम् -करने के लिए, मद्योगम्-मेरे योग (का), आश्रितः- आश्रय लेकर, सर्वकर्मफलत्यागम् -समस्त कर्मों के फल का त्याग, ततः-तब, कुरु-करो, यतात्मवान् - आत्म-संयत होकर ।
अनुवाद : यदि तुम यह भी करने में सक्षम नहीं हो तो मेरे योग के आश्रित हो कर (मेरे साथ एकत्व स्थापित करके), स्वयं को संयत कर के सब कर्मों के फल का त्याग करो (कर्म फल की कामना मत करो)।
व्याख्या यह सरलतम पथ है। यदि तुम कर्म मुझे समर्पित कर के नहीं कर सकते, मेरी सेवा में भी नहीं संलग्न हो सकते, भागवत धर्म भी नहीं जही सकते, अपनी इच्छा से ही प्रेरित हो कर कर्म करना चाहते हो तो मनन बुद्धि को संयत रखने का अभ्यास करते हुए कर्म करो, चाहे अपने लिए ही करो किन्तु कर्तव्य समझ कर करो और मुझे अर्पित करते हुए करो। कर्मफल की भी इच्छा मत करो वह भी मेरे अर्पण कर दो।
श्लोक ८ में ध्यान योग का निर्देशन उत्तम साधकों के लिए है। श्लोक ९ में सतत अभ्यास रूपी योग का उपदेश है। यदि वह भी कठिन लगता हो तो श्लोक १० में बताया गया है कि भगवान् के लिए कर्म करो और जो इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए कर्म-फल-त्याग का संदेश है।
मद्योगम् -मेरा योग। समस्त कर्म और उनका फल मुझे समर्पित करना ही मेरा योग है।
यतात्मवान् - विवेकी पुरुष, जिसने अपनी इन्द्रियों को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध से हटा कर वश में कर लिया है।
अब भगवान् साधकों को कर्मफल त्याग के लिए प्रेरित करने के लिए कर्मफल-त्याग की प्रशंसा करते हैं।
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ।।१२ ।।
शब्दार्थ : श्रेयः-श्रेष्ठ, हि-निस्सन्देह, ज्ञानम् - ज्ञान, अभ्यासात् - अभ्यास से, ज्ञानात् ज्ञान से, ध्यानम् - ध्यान, विशिष्यते-अधिक अच्छा है, ध्यानात् - ध्यान से, कर्मफलत्यागः-कर्मफल का त्याग, त्यागात् त्याग से, शान्तिः शान्ति, अनन्तरम् - अविलम्ब ।
अनुवाद : निश्चित रूप से अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान अधिक अच्छा है, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठतर है, ध्यान की अपेक्षा कर्मफल त्याग प्रशस्ततर है, त्याग से तत्काल शान्ति प्राप्त होती है।
व्याख्या : शास्त्रों से प्राप्त सैद्धान्तिक अथवा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, अज्ञानयुक्त अभ्यास (मन के भावों का नियंत्रण अथवा मूर्ति पूजा अथवा मन और इन्द्रिय जय) की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। सैद्धान्तिक ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठतर है और कर्मों के फल का त्याग ध्यान की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। सर्व कर्मफल त्याग शाश्वत शान्ति (मोक्ष प्राप्ति) का साधन है। अर्जुन को तथा अन्य साधकों को निःस्वार्थ कर्म में प्रेरित करने के लिए और अभ्यास, ज्ञान, ध्यान आदि की अपेक्षाकृत श्रेष्ठता दिखाने के लिए भगवान् कृष्ण ने सर्व कर्मफल त्याग की प्रशंसा की है। जिस प्रकार से ब्रह्मर्षि अगस्त्य के वारिधि जल-पान की बात सुन कर आज के युग के ब्राह्मणों का भी स्तवन होता है क्योंकि अगस्त्य मुनि ब्राह्मण थे, उसी प्रकार साधकों में निष्काम सेवा की प्रबल इच्छा जाग्रत करने के लिए भगवान् कर्मफल त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं।
इच्छा, शान्ति की शत्रु है। इच्छा मन को अशान्त करती है। मनुष्य की समस्त वेदनाओं, दुःखों, समस्याओं का कारण इच्छा है। आत्म-विश्लेषण, अनासक्ति और विवेक द्वारा इच्छाओं के खेल को समाप्त करो। तभी परम शान्ति का आनन्द ले सकते हैं।
साधक के हृदय की पवित्रता के लिए कर्मों के फल के त्याग का निर्देश दिया गया है। यह इच्छा को मार देता है जो ज्ञान का शत्रु है। ज्ञानी ऋषि भी कर्मफल का त्याग करते हैं। उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक है।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ।।१३ ।।
शब्दार्थ : अद्वेष्टा-द्वेष न करने वाला, सर्वभूतानाम् -सब प्राणियों से, मैत्रः-मित्र भाव से 4pi , करुणः सहानुभूति पूर्ण, एव-ही, च-और, निर्ममः- ममता रहित, निरहंकारः- अहंकार रहित, समदुःखसुखः सुख-दुःख में समान, क्षमी क्षमाशील ।
अनुवाद : जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबसे मैत्रीपूर्ण और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करता है, आसक्ति और अभिमान से रहित है और क्षमाशील है,
व्याख्या : आगामी आठ श्लोकों में भगवान् कृष्ण भागवत पुरुष की व्याख्या करते हैं। ये आठ श्लोक 'अमृताष्टकम्' नाम से अभिहित हैं।
ब्रह्म में स्थित भक्त किसी से द्वेषभाव नहीं रखता। वह सब को दया और प्रेम की दृष्टि से देखता है। वह सब में अपना ही रूप देखता है। वह किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रखता। कोई प्राणी उसे कष्ट भी क्यों न दे, वह प्रेम भाव ही रखता है। दीन दुःखियों के प्रति दया भाव रखने वाला और उनको कष्ट से मुक्त करने वाला मनुष्य करुणाशील है। वह स्वयं को दुःखी की अवस्था में रख कर उसके दुःख का अनुभव करता है। दया तो दिव्य गुण है। परमात्मा दयालु हैं। यदि तुम परमात्मा से संलाप करने की इच्छा रखते हो और ब्रह्मत्व पाना चाहते हो तो तुम्हें भी सब के प्रति दयालु होना होगा।
अनन्य भक्त समस्त प्राणियों को अभयदान देता है। वह परमहंस संन्यासी होता है। भगवान् के रहस्यात्मक ढंग तो केवल भक्त ही समझ सकता है। वह सर्वत्र भगवद्दर्शन करता है। सब प्राणियों में उनके दर्शन करता है। तभी तो वह समदृष्टि कहलाता है। वह नदी अथवा सूर्य के समान है। कुटिया हो अथवा राजप्रासाद हो, सूर्य तो सब पर समान प्रकाश विकीर्ण करेगा । नदी का जल कोई भी पी सकता है। गाय हो, सिंह हो अथवा चीता हो, नदी सब की पिपासा शान्त करती है। भक्त के हृदय में 'मैं', 'मेरा' का भाव नहीं होता। यह तेरा है और यह मेरा है-इस प्रकार के भाव भक्त के मन में उदित ही नहीं होते। सुख-दुःख में भी वह समान रहता है, प्रत्युत् सुख-दुःख के प्रति उदासीन रहता है। सुखद विषयों में वह अनुरक्त नहीं होता। दुःखद विषयों से घृणा नहीं करता । पृथिवी के समान वह क्षमाशील होता है। कोई उसका अपमान करे, अपशब्द कहे अथवा उस पर प्रहार भी कर दे, वह अप्रभावित रहता है।
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ।।१४।।
शब्दार्थ : संतुष्टः सन्तुष्ट, सततम् -निरन्तर, योगी-योगी, यतात्मा- आत्म संयत, दृढनिश्चयः - दृढ़ निश्चय वाला, मय्यर्पितमनोबुद्धिः- मुझ में समर्पित मन-बुद्धि वाला, यः जो, मद्भक्तः- मेरा भक्त, सः- वह, मे-मुझे, प्रियः-प्रिय है।
अनुवाद : सदा सन्तुष्ट, ध्यान में स्थिर, आत्म-संयत, दृढ़ संकल्प वाला, जिसके मन और बुद्धि मुझे समर्पित हैं ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है।
व्याख्या: वह जानता है कि इस समय जो कुछ उसे मिल रहा है वह पूर्वकृत् कर्मों का परिणाम है, अतः वह सन्तुष्ट है। वह सीमित, नश्वर पदार्थों की प्राप्ति हेतु संघर्ष नहीं करता। वह अपना मन और बुद्धि परमात्मा में स्थिर रखता है, परम सन्तोष प्राप्त करता है और काल के विपर्ययों में भी चट्टान की भाँति अडिग रहता है।
मेरे भक्त के हृदय में सन्तोष सदा रहता है। सागर की भाँति उसका हृदय सदा परिपूर्ण रहता है क्योंकि उसमें तृष्णा नहीं होती। वह सदा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। शरीर के निर्वाह हेतु भी उसे अनिवार्य सामग्री उपलब्ध हो न हो, वह पूर्णता का ही भाव मन में रखता है उसे अभाव का अनुभव नहीं होता । अच्छी हो बुरी हो, वह अत्यल्प वस्तु में सन्तोष कर लेता है।
शरीर के लिए अनिवार्य-भोजन अथवा वस्त्र के अभाव में भी वह शिकायत नहीं करता, विचलित नहीं होता और कलकल नहीं मचाता। सतत स्थिर मेरे ध्यान के कारण उसका मन सदा पूर्ण रहता है।
योगी-सदा युक्त, सम भाव रहने वाला योगी है। उसने सब इन्द्रियों और इच्छाओं पर विजय पा ली है। पूर्ण आत्म-समर्पण के भाव में उसने दृढ़ संकल्प द्वारा अपने मन और बुद्धि को मुझमें एकाग्र कर लिया है। आत्मा की मूल प्रकृति के विषय में वह दृढ़ संकल्प है। आत्म साक्षात्कार द्वारा जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, "मैं असङ्ग, अकर्ता, शुद्ध सच्चिदानन्द, स्वयंप्रकाश अद्वितीय ब्रह्म हूँ", वह दृढ़ संकल्प वाला ज्ञानी है। उसने पूर्ण रूप से अपना मन (इच्छा और शंका करने वाली शक्ति) और बुद्धि (निश्चयात्मिका शक्ति), मुझे अर्पित कर दिये हैं। वह मुझे उतना ही प्रिय है जितना जीवन । ऐसी उपमा सत्य से कहीं अधिक दूर है अर्थात् असम्भव है।
सप्तम अध्याय में श्लोक १७ में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन से कहा था- "मैं ज्ञानी को बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है", वह बात यहाँ विस्तार से कही गई है।
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ।।१५ ।।
शब्दार्थ : यस्मात् - जिस से, न-नहीं, उद्विजते-उद्विग्न होता है, लोकः संसार, लोकात् संसार से, न-नहीं, उद्विजते-उद्विग्न होता है, च-और, यः-जो, हर्षामर्षभयोद्वेगैः- हर्ष, क्रोध, भय और उत्सुकता से, मुक्तः-मुक्त, यः जो, सः वह, च-और, मे-मुझे प्रियः- प्रिय।
अनुवाद : जिससे किसी लौकिक प्राणी को उद्वेग नहीं होता और जिसे लोक उद्विग्न नहीं कर सकता और जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से रहित है (मुक्त है), वह भक्त मुझे प्रिय है।
व्याख्या : हर्ष-प्रसन्नता, आकाचित पदार्थ की प्राप्ति पर मन की प्रफुल्लित अवस्था । रोमांचित अवस्था और मुख पर अश्रुप्रवाह की अवस्था प्रफुल्लता का संकेत देती है।
अमर्ष-क्रोध । कुछ के अनुसार अमर्ष-क्रोध और ईर्ष्या का मिश्रित भाव है।
उद्वेग-उत्सुकता, चिन्ता, दुःख, व्याकुलता ।
ब्रह्मज्ञानी अथवा भक्त किसी प्राणी को, मनसा, वाचा, कर्मणा कोई कष्ट नहीं पहुँचाता। वह सभी जीवों को अभय और सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए उससे किसी को भय नहीं होता। ज्ञानी यह अनुभव करता है कि संसार उसका शरीर है, उसका अपना ही आत्म तत्त्व है। फिर वह संसार से भयभीत कैसे हो सकता है? न तो वह किसी को कष्ट पहुँचाता है और न ही दूसरों के शब्दों अथवा कर्मों से दुःखी होता है। दावानल अग्नि के समय जिस प्रकार पशु-पक्षी अरण्य त्याग कर चले जाते हैं उसी प्रकार हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग के मानसिक भाव ज्ञानी अथवा भक्त को स्वयं ही त्याग देते हैं।
ऐसा भक्त और ज्ञानी मुझे प्रिय है। उसका वर्णन मैं कैसे करूँ?
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ।।१६ ।।
शब्दार्थ : अनपेक्षः इच्छा मुक्त, शुचिः - पवित्र, दक्षः कुशल, उदासीनः-पक्षपात रहित, गतव्यथः - दुःख रहित, सर्वारम्भपरित्यागी-सब आरम्भों का त्याग करने वाला, यः-जो, मद्भक्तः मेरा भक्त, सः वह, मे मुझे, प्रियः- प्रिय है।
अनुवाद : मेरा जो भक्त इच्छा मुक्त है, पवित्र है, कुशल है, पक्षपात रहित है, दुःखों से मुक्त है, सब आरम्भों का परित्यागी है, वह मुझे प्रिय है।
व्याख्या: वह निर्भरता से मुक्त है, किसी के आधीन नहीं है। वह देह, इन्द्रियों और इन्द्रिय-विषयों के परस्पर सम्बन्ध के प्रति उदासीन है। वह बाहर-भीतर से पवित्र है। बाह्य शुचिता, धावन और मज्जन, पृथ्वी और जल से प्राप्य है किन्तु आन्तरिक शुद्धि राग-द्वेष, तृष्णा, क्रोध, ईर्ष्या आदि से मुक्त होने पर तथा अपने समकक्ष के प्रति मित्रता, निम्न वर्ग के प्रति दया भाव और अपने से श्रेष्ठ के प्रति सम्मान आदि गुणों की नींव डालने से प्राप्त होती है।
दक्ष-कुशल, चतुर, प्रवीण। सब कामों में निपुण। जिन समस्याओं के अविलम्ब ध्यान और कार्य परिणति की आवश्यकता होती है उनका समाधान दक्ष व्यक्ति समुचित रूप से अचिरेण ही कर लेता है।
उदासीन-जो किसी मित्र का पक्ष नहीं लेता; यदि कोई वादानुवाद हो जाये तो वह पक्षपात रहित रहता है।
गतव्यथ-जो पीड़ा से मुक्त है। दुष्ट के प्रहार करने पर भी वह पीड़ित नहीं होता। कोई भी घटना उसे दुःखी नहीं कर सकती।
सर्वारम्भपरित्यागी-इहलौकिक अथवा पारलौकिक, वह स्वभाव से ही मनोरंजन के सब विषयों को प्राप्त करने के लिए कर्म का परित्याग कर देता है। शारीरिक और मानसिक, सभी कर्मों में वह अहंभाव, व्यष्टि भाव और मानसिक प्रेरणाओं से मुक्त हो जाता है। वह अपनी इच्छा भगवान् की इच्छा में मिला लेता है अर्थात् प्रभु जैसा रखें वह उसी में आनन्दित रहता है। दैवी इच्छा उसके द्वारा (उसे निमित्त बना कर) कार्य करती है। न तो उसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा होती है और न ही कोई अपेक्षायें, इसलिए वह सब कर्मों में चतुर, कुशल और निपुण होता है। दैवी इच्छा उसके द्वारा सक्रिय रूप से कार्य करती है।
ऐसा भक्त मेरी आत्मा है अतः वह मुझे प्रिय है।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ।।१७ ।।
शब्दार्थ : य:-जो, न-नहीं, हृष्यति-हर्षित होता है, न नहीं, द्वेष्टि द्वेष करता है, न-नहीं, शोचति-शोक करता है, न-नहीं, काङ्गति-इच्छा करता है, शुभाशुभपरित्यागी-जो शुभ और अशुभ का त्याग करने वाला है. भक्तिमान् भक्तिभाव से पूर्ण, य-जो, स-वह, मे मुझे, प्रिय-प्रिय।
अनुवाद: जो न हर्षित होता है, न घृणा करता है, न शोक करता है और न ही कोई कामना करता है। शुभ-अशुभ का जो परित्यागी है और भक्तिभाव से पूर्ण है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है।
व्याख्या: श्लोक १३ में जो उपेदश दिया गया है वही विस्तार से यहाँ उपदिष्ट है।
कमनीय पदार्थ मिलने पर वह प्रसन्न नहीं होता। अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति पर वह घृणा नहीं करता। अपने प्रिय विषयों के वियोग में वह शोक नहीं करता, अप्राप्त की प्राप्ति की वह कामना नहीं करता।
शुभाशुभपरित्यागी-श्लोक १६ में 'सर्वारम्भ परित्यागी' का ही यह दूसरा निरूपण है। सुख-दुःख देने वाले शुभ-अशुभ कर्मों का त्याग करने वाला भगवान् का भक्त है।
ऐसा भक्त अथवा ज्ञानी जो मेरा आत्म स्वरूप है, मुझे प्रिय है। (निरूपण-VII 17; IX.29)
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।।१८ ।।
शब्दार्थ: सम-सम, शत्रौ-शत्रु में, चऔर, मित्रे-मित्र में, च-और, तथा-भी, मानापमानयो-मान और अपमान में, शीतोष्णसुखदुःखेषु - सदर्दी, गर्मी, सुख-दुःख में, सम-सम, सङ्गविवर्जितः आसक्तिरहित ।
अनुवाद : जो शत्रु और मित्र दोनों के साथ समान व्यवहार करता है, मान-अपमान में समदृष्टि रहता है, सर्दी-गर्मी और सुख-दुखख के द्वन्द्वों में समान रहता है और जो आसक्ति रहित है,
व्याख्या : सामान्य सांसारिक व्यक्ति विरोधी द्वन्द्वों-मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख से प्रभावित होता है किन्तु योगी, ज्ञानी अथवा भागवत पुरुष का मन सन्तुलित रहता है। आकर्षण और विकर्षण की अन्धी शक्तियों के बहाव में वह नहीं बहता।
दूसरों को हानि पहुँचाने वाला व्यक्ति शत्रु है। दूसरों का कल्याण चाहने बाला व्यक्ति मित्र है। भक्त अथवा ज्ञानी को किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती।
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मीनी संतुष्टो येन केनचित् ।
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।।१९ ।।
शब्दार्थ : तुल्यनिन्दास्तुतिः- जो निन्दा और स्तुति को समान समझता है, मौनी-मौन, संतुष्टः सन्तुष्ट, येन केनचित् -किसी भी प्रकार से, अनिकेतः जिसका कोई नियत वास नहीं है, स्थिरमति:-जिसकी बुद्धि स्थिर है, भक्तिमान् - भक्ति भाव से पूर्ण, मे-मुझे, प्रियः- प्रिय, नरः- मनुष्य ।
अनुवाद : जिसके लिए निन्दा और स्तुति समान हैं, जो मौन है अर्थात् वाणी का संयम रखने वाला है, जो कुछ प्राप्त हो उसी में सन्तुष्ट रहता है, जिसका कोई नियत वास नहीं, जिसका मन स्थिर है और भक्ति से पूर्ण है वह मनुष्य मुझे प्रिय है।
व्याख्या : न तो वह स्तुति में प्रमुदित होता है और न ही निन्दा में दुःखी होता है। वह मन की अवस्था को समन्वित रखता है। उसने वाणी पर सयम कर लिया है अतः मौन रहता है। विचारों को संयत कर लेने के कारण उसका मन भी शान्त है सौम्य है। शरीर के निर्वाह के लिए जो भी मिल जाये वह उसी में सन्तुष्ट है। महाभारत के शान्ति पर्व में मोक्ष धर्म पर कहा गया है-जो व्यक्ति शरीर पर जो कुछ मिले धारण कर ले, किसी प्रकार का भोजन जो मिल जाये, स्वीकार कर ले, कहीं भी (जहाँ स्थान मिले) सो जाये उसे देवता ब्राह्मण अथवा जीवन्मुक्त कहते हैं।
वह एक स्थान पर निवास नहीं करता। उसका कोई नियत वास नहीं है। वह बेघर है, वह संसार को ही अपना वास स्थान मानता है। उसका मन सदा ब्रह्म में स्थिर रहता है। (निरूपण - VII. 17, IX.29, XII 17)
ये तु धर्ष्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ।।२० ।।
शब्दार्थ: ये-जो, तु-निश्चित रूप से, धर्ष्यामृतम् - शाश्वत धर्म, नियम, इदम् -यह, यथोक्तम् - जैसा कहा गया है, पर्युपासते-पालन करते हैं, श्रद्धाना - श्रद्धान्वित हो कर, मत्परमा मुझे परम लक्ष्य मान कर, मक्ता, तेवे, अतीव अत्यन्त मे मुझे, प्रिया-प्रिय हैं।
अनुवाद : श्रद्धा से युक्त हो कर, मुझे अपना परम लक्ष्य मान कर जो भक्त उपरोक्त शाश्वत धर्म (नैतिक आचार) का अनुसरण करते हैं वे निथित रूप से मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं।
व्याख्या : इस श्लोक में भगवान् ने उत्कृष्ट भक्त का वर्णन किया है। अमृत धर्म-अमृत जीवन प्रदान करता है, धर्म नैतिकता अथवा ज्ञान है। अभ्यास करने पर धर्म ही अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। सच्चे भक्त मुझे अपना परम गन्तव्य मानते हैं।
इस अध्याय के श्लोक १३ से ले कर २० तक, एक महान् सत्व को प्रकाशित किया गया है जिस पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है, कि भक्त, ज्ञानी और योगी में ये सब विशेषतायें मूल रूप में निहित होती हैं।
'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्' - मैं ज्ञानी को अत्यन्त प्रिय हूँ (VII.17) यह सत्य अत्यन्त विस्तार से निरूपित किया गया है और इन शब्दों में यह उपदेश समाप्त होता है-
तेऽतीव मे प्रियाः
वे मुझे अति ही प्रिय हैं।
जो मनुष्य इस शाश्वत धर्म का पालन करता है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। अतः प्रत्येक साधक जो मोक्ष का पिपासु है और भगवान् के परम धाम का अभिलाषी है, उसे उत्कट उत्साह और निष्ठा से शाश्वत धर्म का पालन करना चाहिए।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ।।१२।।
।। इति भक्तियोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ त्रयोदशोऽध्यायः
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः
अर्जुन उवाच
प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ।
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ।।ॐ ।।
शब्दार्थ : प्रकृतिम् - प्रकृति (पदार्थ), पुरुषम् -पुरुष (आत्मा), च- और, एव-ही, क्षेत्रम् -क्षेत्र, क्षेत्रज्ञम् -क्षेत्र को जानने वाला, एव-ही, च-और, एतत् यह, वेदितुम् - जानने के लिए, इच्छामि-इच्छा करता हूँ, ज्ञानम् -ज्ञान, ज्ञेयम् -जानने योग्य, च-और, केशव-हे केशव ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ।
व्याख्या : कुछ पुस्तकों में यह श्लोक उपलब्ध नहीं है। यदि इस श्लोक को भी लिया जाये तो गीता के पूर्ण श्लोकों की गणना ७०१ हो जायेगी। कुछ टीकाकार इस श्लोक को निवेशित मानते हैं।
अब भगवद्गीता का तीसरा भाग प्रारम्भ हो रहा है। मूलरूपेण तो वही ज्ञान इसमें दिया गया है किन्तु अधिक विस्तृत रूप में है।
निम्न (अपरा) और उच्च (परा), इन दो प्रकृतियों को धारण करने वाले की मूल प्रकृति निश्चित करने के लिए 'क्षेत्र' पर प्रवचन प्रारम्भ किया गया है। इन दोनों प्रकृतियों का वर्णन अध्याय VII के श्लोक ४ और ५ में आ चुका है।
पूर्व अध्याय के श्लोक १३ से अन्तिम श्लोक पर्यन्त 'भगवान् के प्रिय भक्त' के विषय में वर्णन है। अब प्रश्न उठता है-उस भक्त को किस प्रकार का ज्ञान हो ? इसका उत्तर आगे के उपदेश में निहित है।
प्रकृति की रचना तीन गुणों से हुई है। जीवात्मा के दो प्रयोजन-भोग (enjoyment) और अपवर्ग (liberation), पूर्ण करने हेतु प्रकृति स्वयं को देह, इन्द्रियाँ और इन्द्रिय-विषयों में परिणत करती है। सामवेद के महावाक्य-तत् त्वम् असि (तत्त्वमसि) के तीन शब्दों के आधार पर गीता तीन भागों में विभक्त है और प्रत्येक भाग एक-एक शब्द का स्पष्टीकरण करता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रथम छः अध्याय कर्म योग और 'त्वम्' पद का निरूपण करते हैं। आगे के छः अध्याय भक्तियोग अथवा 'तत्' पद को प्रकाशित करते हैं। अन्तिम छः अध्याय ज्ञान योग और 'असि' पद का रहस्य उद्घाटित करते हैं जो 'जीव-ब्रह्म-ऐक्यम्' को स्थापित करते हैं।
अब अर्जुन प्रकृति और पुरुष के मध्य भेद जानने का इच्छुक है। वह इन दोनों का विवेकपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।
श्री भगवानुवाच
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।।१ ।।
शब्दार्थ: इदम् यह, शरीरम्-शरीर, कौन्तेय-हे कुन्ती पुत्र, क्षेत्रम् -क्षेत्र, इति-इस प्रकार, अभिधीयते-कहा जाता है, एतत्-यह, यः जो, वेत्ति-जानता है, तम् - उसे, प्राहुः-कहते हैं, क्षेत्रज्ञः-क्षेत्र को जानने वाला, इति-इस प्रकार, तद्विदः उसे जानने वाले ।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : हे कुन्तीपुत्र (अर्जुन), यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है उसे तत्त्वज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं।
व्याख्या : क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है-खेत। शरीर को क्षेत्र इसलिए कहा है क्योंकि क्षेत्र की भाँति इस शरीर में सुख-दुःख रूपी कर्मों के फल हम प्राप्त करते हैं। भौतिक (स्थूल), मानसिक (सूक्ष्म) और कारण शरीर इस क्षेत्र को पूर्णत्व प्रदान करते हैं। केवल स्थूल शरीर ही क्षेत्र का निर्माण नहीं करता ।
जो व्यक्ति क्षेत्र को जानता है और जो इसे ज्ञान के द्वारा स्वयं से पृथक् देखता है वह क्षेत्र का (पदार्थ का) वेत्ता है।
तद्विदः ऋषि ।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।।२ ।।
शब्दार्थ : क्षेत्रशम् -क्षेत्र को जानने वाला, च-और, अपि-भी, माम् -मुझे, विद्धि -जानो, सर्वक्षेत्रेषु-सब क्षेत्रों में, भारत- हे भरत वंशी (अर्जुन), क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो:- क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, ज्ञानम्-ज्ञान, यत्-जो, तत्-वह, ज्ञानम्-ज्ञान, मतम् माना जाता है, मम-मेरा।
अनुवाद : हे अर्जुन, तुम मुझे सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जानो । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञानी के ज्ञान को मैं वस्तुतः ज्ञान मानता हूँ।
व्याख्या : क्षेत्र पृथक् पृथक् हैं, क्षेत्रज्ञ एक है। व्यष्टि आत्मा (जीवात्मा) अनेक हैं, समष्टि आत्मा (परमात्मा) एक है। जहाँ-जहाँ मन का अस्तित्व है वहाँ वहाँ जीवन है, प्राण है, अहं है और व्यष्टि चेतना अथवा परावर्तित बुद्धि भी है। द्वैत भाव से युक्त व्यक्ति बारम्बार जन्म धारण करता है। ज्ञान-प्रकाश होने पर व्यष्टि आत्मा का समष्टि आत्मा में ऐक्य भाव हो जाता है। द्वैत की भ्रान्ति का निराकरण हो जाता है। "मैं सुखी हूँ", "मैं दुःखी हूँ", "मैं इस कर्म का कर्त्ता हूँ", "मैं अनुभवों का भोक्ता हूँ" -ये मनुष्य के अनुभव मात्र हैं। यही अनुभव लेने अथवा शरीर रूपी कर्मक्षेत्र में अपने कर्मफल भोगने के लिए जीवात्मा संसार के बन्धन में आता है, सुख-दुःख भोगता है और विभिन्न शरीर धारण करता है। किन्तु परमात्मा सुख-दुःख आदि से सर्वथा अतीत है। वह संसार के बन्धन में नहीं आता। वह तो नित्य मुक्त है, अद्वितीय है।
सब शरीरों में यदि आत्मा एक ही है तो सभी को एक समय में एक से अनुभव होने चाहिए। यदि राम उदर-शूल से पीड़ित है तो कृष्ण को भी उसी काल में उसी पीड़ा का अनुभव होना चाहिए। जौन यदि प्रसन्नता का अनुभव करता है तो जैकब को भी वही अनुभव होना चाहिए। चौधरी को यदि बिच्छु ने डंक मारा है तो पीड़ा बैनर्जी को भी वैसी और उसी समय होनी चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं है। राम कष्ट में है तो कृष्ण आनन्द में है। जौन आह्लादित है तो जैकब उदास है। चौधरी बिच्छु के डंक से व्याकुल है तो बैनर्जी प्रातराश (breakfast) के मजे ले रहा है। क्षेत्र पृथक् है, शरीर पृथक् हैं, मन पृथक् है और व्यष्टि आत्मायें भी एक-दूसरे से पृथक् हैं किन्तु इन सब क्षेत्रों में सब का ज्ञाता एक है। सुख और दुःख केवल मन के धर्म हैं। सार रूप में व्यष्टि आत्मा, समष्टि आत्मा से अभिन्न है।
क्षेत्र का ज्ञाता-आत्मा सुख-दुःख, गुण-दुर्गुण से अप्रभावित रहता है। वह केवल मौन द्रष्टा है। सुख-दुःख मन के कार्य हैं। अविद्या के कारण वे आत्मा पर आरोपित हैं। अज्ञानी पुरुष भौतिक शरीर को आत्मा मानता है। राग-द्वेष की दो धाराओं के प्रभुत्व (अधीनता) में रह कर वह शुभ-अशुभ, कर्म कर के इस कर्मक्षेत्र में (शरीर में) सुख-दुःख रूपी फल भोगता है और पुनः जन्म-मरण के चक्र में फंसता है। किन्तु जो ज्ञानी यह जानता है कि क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र को जानने वाला-आत्मा शरीर से पृथक् है वह राग-द्वेष की अधीनता से मुक्त रहता है। वह परमात्मा के साथ युक्त हो कर सदा आनन्द में रहता है और मानवता के कल्याण के लिए निष्काम कर्म में रत रहता है।
तिमिर रोग (आंशिक अन्धापन), जिसमें सत्य के विपरीत दिखाई देता है, आँखों का है किन्तु देखने वाले मनुष्य का नहीं। समुचित चिकित्सा द्वारा यदि रोग हरण हो जाये तो मनुष्य पुनः युक्त देखने लगता है। एवंविध, अविद्या, संशय, सुख-दुःखख, शुभ-अशुभ, राग-द्वेष, मिथ्या दर्शन अथवा उनके कारण, उपादान (मन) से सम्बद्ध हैं मौन साक्षी क्षेत्रज्ञ (आत्मा) से नहीं।
मोक्ष की अवस्था में जहाँ मन (चित्त वृत्ति) का अभाव हो जाता है वहाँ अविद्या और राग-द्वेष की दो धाराओं का अस्तित्व भी नहीं रहता । यदि मिथ्या दर्शन, अविद्या, सुख-दुःख, बन्धन, भ्रान्ति, शोक आदि आत्मा के मूल गुण-सम्पदा होते तो अग्नि में उष्णता के गुण की भाँति उनसे मुक्ति पाना असम्भव था। किन्तु पूर्वकाल में शंकर, दत्तात्रेय, जड़भरत और याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी ऋषि-मुनि हुए हैं जो अलौकिक ज्ञान से युक्त थे और मिथ्या दर्शन,
संशय, भय, भ्रान्ति, शोक आदि से मुक्त थे। उन्हें संसार की चेतना नहीं थी परन्तु स्वरूप जागृति सिद्ध थी। अतः यह सत्य ही है कि आत्मा नित्य मुक्त, शुद्ध-बुद्ध, शाश्वत और पूर्ण है तथा अविद्या मन के आश्रित है, आत्मा के नहीं।
तमोगुण से उद्भुत अविद्या एक आवरण है जो मनुष्य को अपने यथार्थ सच्चिदानन्द स्वरूप को देखने में बाधक है। अविद्या-जनित-दर्शन सत्य के विपरीत होता है और संशय तथा सत्य-दर्शन के अभाव को जन्म देता है। जैसे ही आत्म-प्रकाश का उदय होता है वैसे ही ये तीन प्रकार के अज्ञान पूर्णरूपेण स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वे मन के कारण होते हैं। मन तो अविद्या का एक कार्य रूप है।
संसार चक्र अविद्या के कारण घूम रहा है। यह केवल अज्ञानी मनुष्य के लिए अस्तित्व में है जो इसे वैसे ही देखता है जैसा यह दृष्टिगोचर होता है।
कैवल्य-प्राप्त ज्ञानी के लिए संसार का अभाव हो जाता है। कोई भी चक्षुरोग सूर्य को प्रभावित नहीं कर सकता जो इसका अभिमानी देव है। पात्र-भंजना से बाहर के आकाश अथवा पात्र का भीतरी आकाश प्रभावित नहीं होता। जल मरीचिका धरती को नम नहीं कर सकती। इसी प्रकार अविद्या और इसके प्रभाव शुद्ध, सूक्ष्म, निर्गुण, निराकार, अव्यय, अखण्ड और स्वयं प्रकाश क्षेत्रज्ञ को अल्प मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकते अविद्या आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर सकती । (निरूपण - X.20, XIII.32; XVIII.61)
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत् ।
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ।।३ ।।
शब्दार्थ : तत्-वह, क्षेत्रम् -क्षेत्र, यत्-जो, च-और, यादृक् - जैसा है, च-और, यद्विकारि- जिन विकारों वाला है, यतः- जहाँ से है, च-और, यत्-जो, सः वह, च-और, य-जो, यत्प्रभावः - जिस प्रभाव वाला है, च-और, तत्-वह, समासेन-संक्षेप में, मे शृणु मुझसे सुनो।
अनुवाद : क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके विकार क्या हैं, यह कहाँ से है और कौन है और किन शक्तियों का स्वामी है-ये सब तुम मुझ से संक्षेप में सुनो।
व्याख्या : हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताऊँगा क्षेत्र क्या है, शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसके कौन-कौन से विकार हैं अथवा परिवर्तन हैं। दूसरे शब्दों में, इसमें क्या-क्या परिणति होती है, इसके गुण क्या हैं, किस-किस कारण से क्या-क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, यह किसका है, इसका स्वामी कौन है, यह स्वतः व्युत्पन्नशील है अथवा इसे उत्पन्न किया जाता है।
तत्क्षेत्र-वह क्षेत्र, जिसका विवरण श्लोक १ में आ चुका है। यच्च वह कौन है? उस क्षेत्र को जानने वाला कौन है? उसकी शक्तियाँ क्या हैं? प्रभाव का अर्थ है दर्शन, श्रवण आदि की शक्ति। अब तुम मेरी वाणी से क्षेत्र की यथार्थ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ के विषय में संक्षेप में सुनो।
"मुझे पूर्ण विश्वास है अर्जुन, कि तुम मेरा उपदेश सुन कर सत्य को स्पष्ट रूप से अवधारण करोगे।"
शरीर क्षेत्र है। दस इन्द्रियाँ मानो दस वृषभ हैं। ये वृषभ इन्द्रिय-विषयों के क्षेत्र के माध्यम से अहोरात्र अनवरत रूप से कार्य करते हैं। मन पर्यवेक्षक (superviser) है। जीवात्मा अधिष्ठाता (किरायेदार) है। पाँच प्राण पाँच श्रमिक हैं। आदि प्रकृति क्षेत्र की स्वामिनी है। यह क्षेत्र उसकी सम्पदा है। वह जागरूकता से इस क्षेत्र का प्रतिपालन करती है। प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। रजस् बीज वपन करता है, सत्त्व रक्षण करता है और तमस् फसल काटता है। महत्-तत्त्व (वैश्विक मन) के, धान-मर्दन-क्षेत्र पर काल रूपी वृष की सहायता से आदि प्रकृति धान-मर्दन करती है। यदि जीव अशुभ कर्म करता है तो पाप के बीज वपन करता है, बुराई की खाद से संवर्धन करता है और पाप की फसल काटता है, संसार के दुःखसागर में फंस जाता है अर्थात् जन्म, क्षय, वृद्धावस्था, रोग और तीन प्रकार के क्लेशों को भोगता है। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक ताप सहन करता है। यदि यह शुभ कर्म करता है तो गुण रूपी अच्छे बीज बोता है और सुख की फसल काटता है।
श्रोता में रुचि उत्पन्न करने के लिए अब भगवान् कृष्ण आगामी श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का उत्कृष्ट वर्णन करते हैं।
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ।
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ।।४ ।।
शब्दार्थ : ऋषिभि:- ऋषियों के द्वारा, बहुधा-बहुत प्रकार से, गीतम् - गाया गया, छन्दोभिः वेदमन्त्रों द्वारा, विविधै - विविध, पृथक् -भिन्न, ब्रह्मसूत्रपदै - ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने वाले वचनों (ब्रह्मसूत्रों) द्वारा, छ और, एवं ही, हेतुमद्धि-युक्तियुक्त (वचनों द्वारा), विनिश्थितै-निश्चित ।
अनुवाद: ऋषियों ने इसका गुणगान अनेक प्रकार से, विविध पृथक् बेदमन्त्रों के द्वारा किया है और ब्रह्म को लक्षित करने वाले ब्रह्मसूत्र के पदों में भी युक्तियुक्त ढंग से इसका विवेचन हुआ है।
व्याख्या: वसिष्ठ आदि अनेक ऋषियों ने क्षेत्र की प्रकृति और क्षेत्रज्ञ का वर्णन सनातन काल से किया है। क्रऋग्वेद के सनातन सूक्तों ने इस का विवेचन विविध प्रकार से किया है।
बादरायणाचार्य (व्यास) द्वारा रचित वेदान्त सूत्र ही ब्रह्मसूत्र हैं। उपनिषदों में विपरीत भावात्मक वचनों का विरोध शमन करने हेतु ब्रह्मसूत्र लिखे गये। उपनिषदों का निगूढ़ अलौकिक भाव समझने के लिए ब्रह्मसूत्रों का अध्ययन अनिवार्य है। ब्रह्मसूत्र, शारीरक सूत्र के नाम से भी अभिहित हैं क्योंकि दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के पन्द्रह सूत्र शरीर (क्षेत्र) के विषय में लिखे गये हैं।
क्षेत्र की यथार्थ प्रकृति और इसके ज्ञाता के विषय में ब्रह्मसूत्रों में उपदेश दिया गया है जो ब्रह्म विषयक है जैसे 'आत्मन्येवोपासीत' (बृहदारण्यक, १.४.७) अर्थात् 'आत्मा है', इस प्रकार मनुष्य उस पर ध्यान करे। वे तर्कयुक्त हैं, प्रतीति (अभिज्ञान) कराने वाले हैं और निश्चयात्मक हैं। ब्रह्म विषयक वाक्यों, खण्डों अथवा शब्दों में संशय के लिए स्थान नहीं है।
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ।।५।।
शब्दार्थ : महाभूतानि महाभूत (पँच तत्त्व), अहंकार-अहंकार, बुद्धि-बुद्धि, अव्यक्तम्-अव्यक्त (मूल प्रकृति), एव-ही, च-और, इन्द्रियाणि इन्द्रियाँ, दश-दस, एकम् -एक, च-और, पंच-पॉंच, च-और, इन्द्रियगोचराः इन्द्रियों के विषय ।
अनुवाद : महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल प्रकृति, दस इन्द्रियाँ और एक मन तथा पाँच इन्द्रियों के विषय,
व्याख्या : क्षेत्र और इसके विकार इस श्लोक में बताये गये हैं। सांख्य योग दर्शन के चौबीस तत्त्वों का निरूपण यहाँ किया गया है।
महाभूत-पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश महाभूत कहे गये हैं क्योंकि वे पदार्थ की सब विकृतियों में आच्छादित हैं। यहाँ सूक्ष्म तत्त्वों की ओर संकेत है स्थूल का नहीं।
अहंकार, महाभूतों का कारण है। वह अहंभाव का तत्त्व है। बुद्धि, अहंकार का कारण है। बुद्धि का कार्य है निश्चय करना। बुद्धि संकल्प शक्ति है। अव्यक्त बुद्धि का कारण है। यह भगवान् की अभिन्न शक्ति है। (VII. 14 में भगवान् कहते हैं-दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया-यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया दुस्तर है।)
एकम् - यह मन है। यह ग्यारहवीं इन्द्रिय है और संकल्प-विकल्प इसके कार्य हैं। इन्द्रियों के पाँच विषय हैं-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। ये पाँच इन्द्रियों के भ्रमण स्थल हैं।
महाप्रलय काल में समस्त महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इन्द्रियाँ और मन अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं।
मन माया है। मन अविद्या है। समस्त प्रक्रियाओं के मूल में मन है। मन इच्छाओं को शक्ति देता है, भय का पोषण करता है और हवाई किले बनाता है अर्थात् अपना राज्य चलाता है (मनोराज्यम्) । मन अहं को बल दे कर आकाङ्क्षाओं को प्रेरित करता है। प्रत्येक वृत्ति का जन्म मन से होता है। यह विकारी वृत्तियों का संवर्धन करता है, आशाओं को प्रबल करता है और द्वैत भाव को जन्म देता है। अविद्या को बढ़ाता है और इन्द्रियों को विषयों के सागर में निमज्जित करता है। मन ही भेद भाव और विरोधी वृत्ति का जन्मदाता है। यह पृथक् करता है, विभाजित करता है और सीमित करता है। परमात्मा और जीवात्मा के मध्य मन तो मानो एक प्रबल लौह प्राचीर (दीवार) के समान है। मन ही ब्रह्म को जीवात्मा की स्थिति में लाया है। यह त्रुटियों, तृष्णाओं, संशय, भ्रान्ति और अविद्या का भंडार है। यह नित्य आवर्तनशील चक्र है जो विचारों को उत्पन्न करता है। यह अद्भुत विचार-उत्पादक मशीन है। क्षण भर में विचार सृजित करता है और अगले क्षण नष्ट करता है।
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ।।६ ।।
शब्दार्थ : इच्छा-इच्छा, द्वेष-द्वेष, सुखम् -सुख, दुखम् - दुख, संघात समूह, चेतना-बुद्धि, धृति - धैर्य, एतत्-यह, क्षेत्रम् -क्षेत्र, समासेन-संक्षेप में, सविकारम् - विकारों सहित, उदाहृतम् - वर्णित है।
अनुवाद : इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देह का पिण्ड (शरीर), बुद्धि और स्थिरता-यह संक्षेप में विकारों सहित क्षेत्र का वर्णन है।
व्याख्या : ये तत्त्व आकार बनाते हैं जिन पर इस रूप मय संसार का निर्माण होता है। ये सब मन की अवस्थायें हैं और सांख्य योग दर्शन के अनुसार शरीर की सम्पदा मानी जाती है।
न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये आत्मा के अंतर्जात स्वाभाविक गुण हैं। विकारों का प्रारम्भ है और अन्त भी है। केवल अव्याकृत (अपरिवर्तनशील) ही इन विकारों का साक्षी द्रष्टा हो सकता है। क्षेत्रज्ञ अपरिवर्तनशील है। वह क्षेत्र और इसके विकारों का साक्षी है।
इच्छा मन का विकार है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र लालसा ही इच्छा है। यह रजोगुण से उद्भूत एक वृत्ति (विचार तरङ्ग) है जो मनुष्य को पहले देखी हुई उस वस्तु को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है जिसका सुखद अनुभव वह पूर्वतः प्राप्त कर चुका है। यह अन्तर्मन की सम्पदा है। यह ज्ञातव्य है, अतः क्षेत्र है।
इन्द्रिय-विषय के सुख-भोग का संस्कार अवचेतन मन में रहता है। सुख-भोग की स्मृति से यही संस्कार पुनः सजीव हो उठता है। पुनः उस विषय-भोग की वासना जाग्रत होती है। विषय-भोगों की पुनरावृत्ति, स्मृति और वासना को और प्रचंड (तीव्र) करती है। विषयों के त्याग से और ध्यान के अभ्यास से इच्छायें और संस्कार क्षीण होते हैं।
यदि कोई व्यक्ति बदरी नारायण अथवा माउण्ट कैलाश के सुन्दर दृश्यों का वर्णन करे तो मन में उन स्थानों की यात्रा करने की इच्छा जाग्रत होती है। यदि कोई कहे कि बंगलौर में बहुत अच्छी मिठाई और आम मिल रहे हैं तो तुम्हारे मन में उन्हें प्राप्त करने की लालसा अंकुरित होती है। अतः इन्द्रिय-सुखों की स्मृति और इन्द्रिय-विषयों के गुणों का श्रवण इच्छाओं का मूल कारण है। आशा इच्छा को संवर्धित करती है। आशा इच्छा को नव जीवन प्रदान करती है। इच्छा मन और इन्द्रियों में उत्तेजना उत्पन्न करती है। इच्छा मन को अशान्त करती है। इच्छा मन को विषय-वन में भटकाती है।
इस क्षण जो विषय मधुर और सुखद प्रतीत होता है दूसरे क्षण वही पदार्थ विपरी संवेदना (अनुभव) प्रदान करता है। तुम सब का ऐसा अनुभव रहा होगा । पदार्थ तभी सुखद लगते हैं जब तक उनकी कामना रहती है। कामना न रहे तो वही पदार्थ अच्छे नहीं लगते। इसलिए तथाकथित सुख के मूल में इच्छा निहित है। पदार्थ के सुख भोग से यदि सन्तोष हो जाये तो उस पदार्थ से और अधिक सुख नहीं मिलता। मन यदि इच्छा-मुक्त हो जाये तो तुम सदा विपदा में भी सौम्यता, समचित्तता (समभाव) और शान्त भाव का आनन्द लोगे। इन्द्रिय-विषयों से प्रेम इच्छा की आधारशिला है। इच्छायें तुम्हारी प्रवृत्ति प्रवाह, भाव और रुचि के पथ पर दौड़ती हैं। इच्छा ईंधन है। विचार अग्नि है। यदि तुम इच्छा रूपी ईंधन को समाप्त कर दो तो तेल-रहित लैम्प की भाँति विचार की अग्नि शान्त हो जायेगी, बुझ जायेगी। इच्छाओं की संगति में बुद्धि अपवित्र होती है।
घृणा मन की एक वृत्ति है जो नकारात्मक है। किसी वस्तु अथवा जीव विशेष से कभी पीड़ा का अनुभव हुआ हो तो उसके प्रति घृणा अथवा अरुचि के लिए यह वृत्ति मन को प्रेरित करती है, जब भी वह पुनः उसको देखता है। घृणा भी क्षेत्र है क्योंकि यह ज्ञातव्य है। इच्छापूर्ति के अभाव में मन में उत्पन्न होने वाली भावना ईर्ष्या अथवा घृणा है। सुख रुचिकर, शान्तिप्रद और सत्त्व निर्मित है। यह भी क्षेत्र है क्योंकि यह ज्ञातव्य है । दुःख अरुचिकर और क्लेशप्रद है। यह भी क्षेत्र है क्योंकि यह भी ज्ञातव्य है।
सङ्घात-समूह-इन्द्रियों और शरीर का पिण्ड अथवा शरीर के ३५ घटकों का समूह ।
चेतना-लोहे की गेंद में अग्नि की अभिव्यक्ति की भाँति चेतना एक मानसिक अवस्था है जो अपने को समग्रता में अभिव्यक्त करती है। यह भी क्षेत्र है क्योंकि यह ज्ञातव्य है। चेतना जीवनी शक्ति अथवा प्राण वायु है।
धृति-दृढ़ता, साहस, सहनशीलता। यह मन की सात्विक वृत्ति है। शरीर, मन और इन्द्रियों की क्षुब्ध और विषाद की अवस्था में धृति धारण से शक्ति आती है। पाँचों तत्त्व एक-दूसरे के विरोधी है। जल पृथ्वी को नष्ट करता है. अग्नि जल को सुखाता है, जल अग्नि को बुझाता है। वायु दीप (अग्नि) को बुझाता है और आकाश वायु को अपने में लीन कर लेता है। पाँचों तत्त्व आपस मैं विरोधी हैं, स्वभाव से ही एक दूसरे के शत्रु हैं पुनरपि इसी शरीर में वे सब कितने मित्रभाव से मिलकर रहते हैं। शरीर का कोई भी व्यापार (क्रिया) समन्वित रूप से पूर्ण करने के लिए प्रत्येक तत्त्व बहुत सुन्दर रूप से अन्य तत्वों का साथ देता है। धृति वह शक्ति अथवा दृढ़ निश्चय है जिसके द्वारा ये युयुत्सु तत्व भी एकता और समन्वय के साथ स्थिर और सन्तुलित रखे जाते हैं। यह भी क्षेत्र है क्योंकि ज्ञातव्य है।
इस श्लोक में वर्णित इच्छा आदि गुण मन के समस्त गुणों को लक्षित करते हैं। प्रथम श्लोक में जिस क्षेत्र का वर्णन किया गया है, पंचम और षष्ठ श्लोकों में इन्हें पूर्ण विस्तारपूर्वक समझाया गया है।
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ।।७ ।।
शब्दार्थ : अमानित्वम् नम्रता (अभिमान का अभाव), अदम्भित्वम् - दम्भाचरण (छल-कपट) का अभाव, अहिंसा-अहिंसा, क्षान्तिः- क्षमा, आर्जवम् - सरलता, आचार्योपासनम् - गुरु सेवा, शौचम् - शुद्धता (शरीर और मन की), स्थैर्यम् -स्थिरता, आत्मविनिग्रहः- आत्म-संयम ।
अनुवाद : नम्रता, दम्भाचरण का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, शुचिता, स्थिरता, आत्म-संयम,
व्याख्या : बुद्धिमान् में अथवा बुद्धिमान् बनने के लिए ये गुण आवश्यक हैं। अन्तश्चेतना की ओर उन्मुख मन वाले व्यक्ति की ये उपाधियाँ हैं।
यदि से समस्त गुण किसी में समग्रता से दृष्टिगत हों तो अनुमान लगा ले कि आत्म ज्ञान का सूर्य उस व्यक्ति में उदित हो गया है।
अमानित्वम् - यह अहंकार (मिथ्याभिमान) का अभाव है। आत्मश्लाघा की शून्यता है। धन-वैभव, ज्ञान, बल, सौन्दर्य तथा अन्य गुण दूसरों की अपेक्षा अपने में अधिक होने की चेतना, मिथ्या अभिमान का आधार हैं। अभिमानी के पास पुनरपि, कुछ न कुछ तो होगा किन्तु अहंकारी के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वह सोचता है वह दूसरों से श्रेष्ठ है। अतिशय अभिमान मानित्व है। एक नम्र व्यक्ति को आदर, सम्मान और प्रशंसा की आकाङ्क्षा नहीं होती। वह प्रशंसा और भेदभाव की वृत्ति का त्याग करता है। वह अपने ज्ञान, योग्यता और शक्ति आदि का दिखावा नहीं करता। आत्मश्लावा नहीं करता।
अदम्भित्वम् - जो तुम हो नहीं वह दिखना चाहते हो-यह दम्भाचरण कहलाता है। किसी संन्यासी के पास कुछ गुण हैं और पुस्तकों से अर्जित कुछ सैद्धान्तिक ज्ञान । किन्तु वह मुक्त संन्यासी होने का ढोंग करे तो वह दम्भी है। यह धार्मिक दम्भ (पाखण्ड) है। दम्भ के अभाव में मनुष्य सरल और नम्र होता है। दूसरों से आदर, नाम और स्तुति प्राप्त करने के लिए वह अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करता । अपने किये हुए प्रशस्य अथवा दानशील कार्य को वह प्रकट नहीं करता। वह पांडित्यदर्शन (विद्याभिमान) से मुक्त होता है। प्रशंसा प्राप्ति के लिए वह अपने ज्ञान का विक्रय नहीं करेगा।
अहिंसा-मनसा, वाचा, कर्मणा किसी प्राणी को कोई कष्ट न पहुँचाना, अहिंसा है। अहिंसा का पालन करने वाला अत्यन्त ध्यानपूर्वक धरती पर पाँव रखता है ताकि उसके पाँव तले कोई जीव कुचल न जाये। किसी जीव को देख लेगा तो दूसरी ओर मुड़ जायेगा। उसका हृदय करुणामय होता है।
क्षान्ति-सहिष्णु, तितिक्षु, क्षमाशील व्यक्ति वही है जो क्षान्ति से युक्त है। यह ज्ञान का सत्य लक्षण है। ज्ञानी पुरुष सब कुछ सहन करता है। दूसरे उसे चोट भी क्यों न पहुँचायें वह अप्रभावित रहता है। वह कोई प्रतिक्रिया अथवा प्रतिहिंसा नहीं करता। वह शान्त भाव से अपमान और हिंसा सहन करता है।
आर्जवम् -सरलता । ज्ञानी पुरुष सरल होता है। वह छल-कपट, कुटिलता, धूर्तता और प्रवंचना से परे रहता है। वह स्पष्टवादी और सहृदय होता है। वह किसी से कुछ छिपाता नहीं अर्थात् रहस्य नहीं रखता। उसके वाणी और विचार में समता होती है। वह अपने मन की बात लोगों से स्वतन्त्र रूप से कह देता है। वह बोलने में बालक की भाँति सरल होता है। स्फटिक की भाँति शुद्ध हृदय होता है। वह दूसरों को कभी धोखा नहीं देता।
गुरु सेवा-आचार्य के प्रति भक्ति भाव, गुरु पूजा, ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाले अथवा मोक्ष का साधन बताने वाले की सेवा (उपासना) गुरु सेवा है। दिव्य ज्ञान स्वरूप शिक्षक ही आचार्य है। गुरु सेवा से साधक को मोक्ष श्रीति का साधन मिलता है। साधक अपने गुरु की ब्रह्म भाव में पूजा करता है। बह उसकी विष्णु रूप में स्तुति करता है। वह गुरु पर ब्रह्म अथवा विष्णु की अहस्त उपाधियाँ अधिष्ठित करता है। वह गुरु में और गुरु के द्वारा ब्रह्म का हसाक्षात्कार करता है। यह गुरु सेवा का फल है। वेदान्त के साधक के लिए गुरु शक्ति अनिवार्य है। शास्त्रों का गोपनीय अर्थ जानने के लिए भी गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है।
शौच-शुचिता, पवित्रता । यह अन्तः और बाह्य, दो प्रकार की है। बाह्य पवित्रता भौतिक शरीर की है जो मृत्तिका (मिट्टी) और जल से होती है। दूसरी शुद्धि अन्तःकरण की है जिस पर घृणा, ईर्ष्या-द्वेष और आसक्ति का मल बढ़ा हुआ है। इसे प्रतिपक्ष भावना से अर्थात् सकारात्मक गुणों के द्वारा और विषय-वासनाओं में दोष दृष्टि रखने से शुद्ध किया जाता है।
स्थैर्यम् - स्थिरता । साधना की राह में अनेक बाधायें आने पर भी साधक अपने निर्वाण-पथ पर संघर्ष करता हुआ आगे ही बढ़ता है। यह स्थिरता और दृढ़ता है। चंचल मन से ब्रह्म पर ध्यान करना असम्भव है।
विनिग्रहः यह इन्द्रियों और शरीर का समग्रता से संयम है। इन्द्रियाँ और शरीर जो स्वभावतः बहिर्मुख होते हैं और विषयों की ओर दौड़ते हैं, इन्हें वश में कर के निर्वाण-पथ पर स्थिर किया जाता है। इन्द्रियाँ असंयत हों और ध्यान आकृष्ट करती हों, ऐसे शरीर में ध्यान सम्भव नहीं है।
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ।।८ ।।
शब्दार्थ : इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियों के विषयों में, वैराग्यम् - विरक्ति, अनहकार-अहंकार का अभाव, एव-ही, च-और, जन्ममृत्युजराव्याधि- दुःखदोषानुदर्शनम् जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःख में दोष देखना ।
अनुवाद : इन्द्रिय-विषयों में वैराग्य और अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःख में दोष दर्शन,
व्याख्या : बुद्धिमान् पुरुष इन्द्रिय-विषयों के प्रति सदा विरक्त रहता है। उनके विषय में कुछ बोलना भी उसे प्रिय नहीं है। उसकी इन्द्रियाँ विषयोन्मुख नहीं होतीं।
वैराग्यम् - शब्द, स्पर्श आदि, दृष्ट अथवा अदृष्ट, श्रुत अथवा अश्रुत सुख के प्रति अनासक्ति का भाव वैराग्य है चाहे वह स्वर्गलोक का भी क्यों न हो।
अनहंकार-"मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ"-मन का यह भाव अहंकार है। इस भाव का अभाव अनहंकार है।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्-गर्भ में नौ मास पर्यन्त वास कर के जन्म के दुःख सहन करने पड़ते हैं। यह जन्म के पाप हैं। बुद्धिमान् व्यक्ति जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि के क्लेशों को कभी विस्मृत नहीं करता। वह जन्म से मुक्ति चाहता है। वृद्धावस्था में बुद्धि मन्द हो जाती है, स्मृति-हास हो जाता है, इन्द्रियाँ क्षीण हो जाती हैं। शक्ति और बल का क्षय होने लगता है। अपने सम्बन्धियों के द्वारा वृद्ध हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये वृद्धावस्था की बुराइयाँ हैं, दोष हैं। अर्श रोग (piles) से पीड़ित व्यक्ति दुर्बलता का अनुभव करता है, रक्त क्षय के कारण उसे अनीमिया हो जाता है। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति की तिल्ली बढ़ जाती है। यह व्याधि दोष हैं।
दुःख-ग्रन्थ के आरम्भ में तापत्रय का वर्णन आ चुका है। दुःख स्वयं में ही एक दोष है। जन्म दुःख रूप है, जन्म दुःख है, मृत्यु दुःख है, जरा दुःख है, व्याधि दुःख है। जन्म, मृत्यु आदि सब दुःख रूप हैं क्योंकि ये सब दुःख देते हैं।
इन सब में इस प्रकार का दोष दर्शन और विश्लेषण करने से शरीर और इन्द्रियों के सुखों के प्रति वैराग्य का भाव जाग्रत होता है। तब मन अन्तर्मुखी हो कर आत्म-ज्ञान के लिए तड़पता है। क्योंकि जन्म आदि में दुःख दोष दर्शन करने से आत्म-ज्ञान की प्राप्ति में सहायता मिलती है अतः यह भी ज्ञान है।
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।।९ ।।
शब्दार्थ : असक्तिः - अनासक्ति, अनभिष्वङ्गः - देहाभिमान का अभाव, मोह ममता आदि का अभाव, पुत्रदारगृहादिषु-पुत्र, स्त्री, गृह आदि में, च-और, समचित्तत्वम् -चित्त नित्यम् -सदा, इष्टानिष्टोपपत्तिषु अभीष्ट और अनभीष्ट की प्राप्ति में। का सम रहना,
अनुवाद : अनासक्ति, पुत्र, दारा, गृह आदि में मोह-ममता और एकत्व भाव का अभाव, अभीष्ट और अनभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति पर समचित्तता,
व्याख्या : जब मनुष्य सोचता है, "यह वस्तु मेरी है", "मैंपन का भाव उसके चित्त में प्रविष्ट होता है। उसमें अभिमान का विकास होने लगता है और वह वस्तुओं से (एकत्व स्थापित कर) प्रेम करने लगता है। उनमें आसक्त हो जाता है। विषयों में आसक्ति का अभाव अनासक्ति है। यह विषयों में रुचि का अभाव है।
अनभिष्वङ्गः -पुत्र, दारा, माता आदि में प्रगाढ़ आसक्ति का अभाव है। यहाँ आत्मा का दूसरे के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। दूसरे के सुखी-दुःखी होने पर वह भी सुखी-दुःखी होता है। गोविन्दन् अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी मृत्यु होने पर वह बहुत शोक ग्रस्त हो गया किन्तु उसके पड़ोसी की पत्नी का देहान्त हुआ तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्ञानी पुरुष को अपने घर से कोई आसक्ति नहीं होती। राजमार्ग (Public Road) के किनारे बसे अपने आवास को वह एक अतिथि गृह ही मानता है।
आदिषु-अन्य प्रिय जन । सम्बन्धी अथवा सेवक ।
नित्यं समचित्तत्त्वम् समता ज्ञान की अनुक्रमणिका है। अभीप्सित पदार्थ की प्राप्ति पर ज्ञानी पुरुष हर्षित नहीं होता और अनभीप्सित में दुःखी नहीं होता ।
अनासक्ति, राग का अभाव और समत्व, आत्म-ज्ञान प्राप्ति में सहायक गुण हैं। वे गुण ज्ञान की संज्ञा से अभिहित हैं क्योंकि वे ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं।
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।।१०।।
शब्दार्थ: मयि मुझ में, चऔर, अनन्ययोगेन-अनन्य योग के द्वारा, भक्ति -भक्ति, अव्यभिचारिणी-अविचल, विविक्तदेशसेवित्वम् - एकान्त देश (स्थान) में निवास करना, अरति-अरुचि, जनसंसदि -मानव समाज में।
अनुवाद : मुझ में अनन्य भाव से अविचल भक्ति, एकान्त-वास और मानव समाज के प्रति अरुचि अर्थात् अनुराग का अभाव,
व्याख्या : ज्ञानी पुरुष दृढ़तापूर्वक इस सत्य को स्वीकार करता है कि
मैं ही सब का केवल आधार (आश्रय) हूँ और मुझ से श्रेष्ठ और कोई नहीं। किसी अन्य विषय का विचार मन में न लाते हुए वह (योग के द्वारा) मेरे में ही अचल निष्ठा रखने वाला होता है। उसका चित्त मुझ में लीन हो गया है। जैसे नदी सागर में मिल कर उससे एक रूप हो जाती है वैसे ही वह मेरे साथ युक्त हो कर केवल मेरी ही उपासना करता है। अनन्य योग अथवा अपृथक् समाधि यही है। ऐसी ही भक्ति ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। ऐसा भक्त अनेक विपदाओं और परीक्षाओं में संघर्ष करते हुए भी अपनी भक्ति और पूजा को नहीं छोड़ेगा।
विविक्तदेशसेवित्वम् - वह पावन नदियों के तट पर वास करेगा, पर्वत की गुहाओं में, सागर-तट पर अथवा झील के किनारे और एकान्तदेशी सुन्दर उद्यानों में रहेगा जहाँ सर्प, सिंह और चोर आदि का भय न हो। एकान्त स्थान में चित्त शान्त रहता है। ऐसे स्थानों पर ध्यान आकृष्ट करने वाले बाधक तत्त्व नहीं होते। आत्मा पर अनवरत रूप से दीर्घावधि पर्यन्त ध्यान कर के अचिरेण समाधि की अवस्था प्राप्त की जा सकती है।
जनसंसदि-यहाँ सांसारिक व्यक्तियों की समाज से दूरी रखने का आदेश है, बुद्धिमान्, पवित्र और साधु पुरुषों से नहीं। विद्वानों की सङ्गति आत्म-ज्ञान का साधन है।
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।।११ ।।
शब्दार्थ : अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्-आत्म-ज्ञान में नित्य स्थिति, सत्वज्ञानार्थदर्शनम् - परम सत्य की दार्शनिक खोज, एतत्-यह, ज्ञानम् - ज्ञान, इति-इस प्रकार, प्रोक्तम् -घोषित किया गया है, अज्ञानम्-अज्ञान, यत् जो, अत-इससे, अन्यथा अन्य, इतर ।
अनुवाद : आत्म-ज्ञान में नित्य स्थिति और परम सत्य की खोज के लिए अन्तदृष्टि-यह ज्ञान कहा गया है और इससे इतर जो कुछ भी है, वह अज्ञान है।
व्याख्या : मुक्तात्मा में सदा आत्म जागृति बनी रहती है। वह जानता है कि अध्यात्म ज्ञान ही नित्य है और शेष समस्त ज्ञान जो संसार से सम्बद्ध है, वह अज्ञान है। वह जानता है कि आत्मदर्शन कराने वाला ज्ञान ही केवल सच्चा ज्ञान है।
'नम्रता' के गुण से प्रारम्भ हो कर ये सभी गुण ज्ञान के अन्तर्गत घोषित किये गये हैं क्योंकि वे ज्ञान के अनुरूप हैं, वे ज्ञान के साधन हैं, वे ज्ञान के गौण साधन स्वरूप अथवा उपादान कारण हैं। इस आत्म-ज्ञान का परिणाम जन्म-मृत्यु के चक्र से मोक्ष है। आध्यात्मिक साधक को इस प्रकार से ज्ञान की पराकाष्ठा को सदा स्मरण रखना चाहिए। तभी वह उन गुणों का विकास कर सकता है जो निर्वाण प्राप्ति में सहायक हैं। ज्ञान के विपरीत-काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दम्भ, आसक्ति, धृष्टता, कूटनीति, हिंसा का भाव (दूसरों को चोट पहुँचाना), आदि अज्ञान है। अज्ञान से उत्पन्न ये दुर्गुण मनुष्य को भौतिक बन्धन में डालते हैं। मोक्ष-प्राप्ति के इच्छुक साधक को अज्ञान के ये प्रतिबन्धक मार्ग से हटाने होंगे। विपरीत गुणों का विकास कर लो, बुरे गुण उसी प्रकार अस्तित्व खो देंगे जैसे उद्यान में बिना जल के पौधे । दुर्गुणों से लड़ते हुए उनका निराकरण करना किंचित् कठिन है।
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।।१२ ।।
शब्दार्थ : ज्ञेयम् - जानने योग्य, यत्-जो, तत्-वह, प्रवक्ष्यामि - कहूँगा, यत्-जो, ज्ञात्वा-जान कर, अमृतम्-अमरत्व, अश्नुते - (कोई भी) प्राप्त करता है, अनादिमत् - अनादि, परम् -परम, ब्रह्म-ब्रह्म, न-नहीं, सत् सत्, न-नहीं, असत् - अस्तित्व कान (न होना), उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : अब मैं ज्ञातव्य की घोषणा करूँगा जिसे जान कर मनुष्य अमृतत्व की प्राप्ति करता है, वह अनादि परम ब्रह्म न तो सत् कहा जाता है और न ही असत् ।
व्याख्या : अर्जुन में अथवा किसी भी श्रोता के हृदय में उसे जानने की उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए भगवान् उस परब्रह्म परमात्मा की प्रशंसा करते हैं जो जानने योग्य है।
ब्रह्म को सत् अथवा असत् आदि शब्दों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह किसी भी प्रकार की जाति-ब्राह्मण, गाय, घोड़ा आदि से परे है। उसके श्वेत, श्याम आदि वर्ण भी नहीं हैं। उसका किसी अन्य वस्तु से सम्बन्ध अथवा सम्पर्क भी नहीं है क्योंकि वह अद्वितीय है। यह किसी इन्द्रिय का विषय नहीं है। इसे मन और इन्द्रियों द्वारा जानना असम्भव है। यह निष्क्रिय है। यह महान् भावातीत (अलौकिक), अव्यक्त परम ब्रह्म है। सभी विषयों में यह साक्षी चेतन कर्त्ता है।
वेद गौरव के साथ उद्घोष करते हैं कि ब्रह्म, अकर्ता, अभोक्ता और अव्यय है। अध्याय IX. 19 में कहा गया था कि वह सत् भी है और असत् भी। अब भगवान् कह रहे हैं कि वह न तो सत् है और न असत् । अध्ययनकर्ता को यह विरोधी बात प्रतीत हो सकती है किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। यद्यपि व्यक्त (मर्त्य) और अव्यक्त (अमर्त्य) ब्रह्माण्ड ब्रह्म स्वरूप ही हैं तथापि वह इन दोनों से अतीत है। (VII.2; XV.16, 17, 18)
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।।१३ ।।
शब्दार्थ : सर्वतः सब ओर, पाणिपादम् -हाथ और पाँव सहित, तत् वह, सर्वतः सब ओर, अक्षिशिरोमुखम् - आँख, सिर और मुख वाला, सर्वतः सब ओर, श्रुतिमत् -कर्णयुक्त, लोके-लोक में, सर्वम्-सब, आवृत्य-आवृत कर के, तिष्ठति-रहता है।
अनुवाद : उसके हाथ-पैर सब ओर हैं, नेत्र, सिर और मुख सब ओर हैं, कर्ण सब ओर हैं, वह लोक में सब को आवृत कर के, सबको व्याप्त कर के स्थित है।
"व्याख्या : वह (क्षेत्रज्ञ अथवा परब्रह्म) संसार में सर्वत्र व्याप्त है। वह स्वयं से समस्त संसार को पूर्ण करता है और सब ओर से परिवेष्टन करता है। वह लोक में सर्वस्व आच्छादन कर के स्थित है।
पूर्व श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्म जो ज्ञेय है, न तो सत् है और न वह असत्। ऐसा विचार आ सकता है कि वह असत् होगा, शून्य होगा अब मिथ्यार्थबोध (मिथ्या-अर्थबोध) को दूर करते हुए भगवान् इस श्लोक में कहते ● हैं कि ज्ञान के सर्वत्र हाथ-पैर आदि हैं। इससे मन और इन्द्रियों को समुचित बेष्टा करने हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होता है। यह केवल ब्रह्म के सगुण स्वरूप का पक्ष है।
जिस प्रकार से इंजन का ड्राइवर इंजन को चलाता है उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ शरीर रूपी इंजन को चलाता है। यह अन्तः शासक है, अन्तस्तम आत्मा है। इन्द्रियों, प्राणशक्ति, मन, शरीर और संसार का यह अवलम्बन है, आधार है। शरीर, मन और इन्द्रियों के सीमित प्रतिबन्धों के अस्तित्व का आधार अथवा निश्चितता, ब्रह्म है क्योंकि इन सब की प्रक्रियाओं के पीछे आत्म चेतना का अस्तित्व अनिवार्य है तो इसे असत् कैसे कह सकते हैं?
रज्जु पर अध्यासित सर्प के गुण-दोषों से जैसे रज्जु अप्रभावित रहती है उसी प्रकार परब्रह्म (क्षेत्रज्ञ) अध्यासित शरीर, मन, इन्द्रियाँ, प्राण शक्ति और संसार से प्रभावित नहीं होता। सब जीवों में सामान्य चेतना एक ही है। वह सामान्य चेतना शाश्वत, स्वयं प्रकाशित और सर्वव्याप्त है। वह सामान्य चेतना परब्रह्म है। शरीर, मन, इन्द्रियाँ और प्राण स्वभाव से जड़ हैं किन्तु ब्रह्म की शक्ति से वे गति करते हैं। वे ब्रह्म (क्षेत्रज्ञ) के कारण ही गतिशील हैं। सीमित प्रतिबंध भ्रम मात्र है। अतः वे चेतना की आभा धारण किये हुए हैं। चुम्बक के संयोग से जैसे लोहा, सादृश्यता को प्राप्त होता है उसी भाँति यह संसार चेतना के संयोग में चैतन्य ही आभासित होता है।
रज्जु में सर्प की भाँति यह संसार ब्रह्म पर अध्यासित है। इस अध्यारोपण कहते हैं। अपवाद (negation) की युक्ति से इसे अध्यारोपण स मुक्त अथवा संशोधित कर सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं।
यह भाव श्वेताश्वतरोपनिषद ३.१६ से उद्धृत है।
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ।।१४ ।।
शब्दार्थ : सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सब इन्द्रिय-वृत्तियों के रूप में अवभासित, सर्वेन्द्रियविवर्जितम् -सब इन्द्रियों से रहित, असक्तम्-अनासक्त, सर्वभूत् -सब का पालन करने वाला, च-और, एव- ही , निर्गुणम्-उपाधि रहित, गुणभोक्तृ-(पुनरपि) गुणों का भोक्ता, चऔर।
अनुवाद : वह समस्त इन्द्रियों के गुणों के द्वारा अवभासित होता हुआ भी सब इन्द्रियों से रहित है। अनासक्त होते हुए सब का पोषण करता है। निर्गुण होते हुए गुणों का भोक्ता है।
व्याख्या : ब्रह्म बिना चक्षु के दर्शन करता है, बिना श्रोत्र के श्रवण करता है, बिना नासिका के घ्राण करता है, बिना मुख के भोग करता है, बिना त्वचा के अनुभव करता है, बिना हाथों के ग्रहण करता है, बिना चरण के गमन करता है। "वह अदृश्य द्रष्टा है, अश्रुत श्रोता है, अचिन्त्य चिन्तन है। उससे भिन्न कोई अन्य द्रष्टा नहीं, श्रोता नहीं और चिन्तक (मन्ता) नहीं। वह आत्मा है, अन्तर्यामी नियामक है और नित्य है।" (बृहदारण्यकोपनिषद् III.7.23) प्रकृति के गुणों से मुक्त होते हुए भी उनका भोक्ता है।
सर्वेन्द्रियः -पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ । मन और बुद्धि भी इन्द्रियों के अन्तर्गत परिभाषित हैं। मन और बुद्धि की सहायता से ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ कर्म करती हैं। उनकी स्वतन्त्र चेष्टा नहीं होती। इसीलिए मन और बुद्धि भी इन्द्रिय समुदाय में सम्मिलित हैं।
ब्रह्म अव्यक्त और भावातीत है किन्तु अन्तः और बाह्य इन्द्रियों के माध्यम से वह अपने को व्यक्त करता है। इन्द्रियातीत होने से वह अनासक्त है पुनरपि सब का पोषण करता है। वह सब का अधिष्ठान है। निर्गुण होते हुए (गुणातीत होते हुए) भी वह प्रकृति के गुणों का भोक्ता है। ब्रह्म वस्तुतः रहस्यमय है। यह भाव श्वेताश्वतरोपनिषद् ३.१७ से लिया गया है।
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ।।१५ ।।
शब्दार्थ : बहिः- बाहर, अन्तः-भीतर, च-और, भूतानाम् -प्राणियों के, अत्तरम् -स्थिर (जड़), चरम् - गतिशील (चेतन), एव-ही, च-और, सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मता के कारण, तत्-वह, अविज्ञेयम्-अज्ञेय, दूरस्थम् - दूर, -और, अन्तिके समीप, च-और, तत्-वह।
अनुवाद : समस्त चराचर प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान होते हुए भी सूक्ष्मता के कारण जो अज्ञेय है वह दूर भी है और पास भी है।
व्याख्या : आकाश की भाँति ब्रह्म सूक्ष्म है। अत्यन्त सूक्ष्म होने से यह अज्ञानियों के लिए अगम्य है। मोक्ष के साधन चतुष्टय से अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए यह अज्ञेय है। (III.3)
विद्वानों द्वारा ब्रह्म ज्ञेय है। साधन चतुष्टय में कुशल साधक ही इसका साक्षात्कार कर सकता है। विद्वान् का आत्मा होने के कारण वह उसके अत्यन्त समीप है। विषयों में निमग्न सांसारिक पुरुष से वह अत्यन्त दूर है। अज्ञान-अन्धकार में पड़े हुए, अविद्या से आच्छादित मनुष्य को वह कोटि- कोटि वर्षों में भी प्राप्य नहीं है।
दूरस्थं चान्तिके-यही भाव ईशावास्योपनिषद् के मन्त्र ५, और मुण्डकोपनिषद् में ३/१/७ में देखा जा सकता है।
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।। १६ ।।
शब्दार्थ : अविभक्तम् - विभाग रहित, च-और, भूतेषु प्राणियों में, विभक्तम् -विभक्त, इव-समान, च-और, स्थितम् -स्थित है, भूतभर्तृ- प्राणियों का पोषण करने वाला, च-और, तत्-वह, ज्ञेयम्-जानने योग्य, प्रसिष्णु-संहारकर्त्ता, प्रभविष्णु-उत्पन्न करने वाला, च-और।
अनुवाद : अविभक्त होते हुए वह प्राणियों में विभक्त सा प्रतीत होता है। उसे प्राणियों के पोषणकर्ता, संहारकर्ता और उत्पन्नकर्ता के रूप में जाना ज सकता है।
व्याख्या : ब्रह्म को सृष्टिकर्ता, पालनकर्त्ता और संहारकर्ता के रूप में जानना चाहिए। इन तीन रूपों में वह नाम-रूप का संसार सृजित करने वाला ब्रह्मा है, रक्षण पोषण करने वाला विष्णु और संहारकर्ता के रूप में वह रुद्र है। यह विभिन्न शरीरों में अविभाज्य है। इसकी उपमा आकाश से दी जा सकती है। आकाश की भाँति यह सर्वव्यापक है। यह अविभाज्य और एक है, अद्वितीय है किन्तु रूपों में विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है और सब वस्तुओं और जीवों में पृथक् पृथक् सा अवभासित होता है। मूलतः अखण्ड होते हुए भी समस्त प्राणियों में विभक्त हुआ भासता है।
महाप्रलय में यह संसार को विलीन कर देता है। अगले कल्प में पुनः इसका सृजन करता है। संसार की पोषण की अवधि में वह सबका पोषण करता है।
काष्ठ में निहित अग्नि की भाँति ब्रह्म सब शरीरों में विद्यमान है। एक आकाश जैसे सीमित प्रतिबन्धकों के कारण पृथक् पृथक् प्रतीत होता है (पात्र आदि में), वैसे ही एक अविभाज्य ब्रह्म शरीर आदि सीमित प्रतिबन्धों के कारण पृथक् प्रतीत होता है।
एक आलोचक का कथन है- "ज्ञेय ब्रह्म जो क्षेत्रज्ञ है, सर्वव्यापक है, वह सर्वत्र विद्यमान है और फिर भी दिखाई नहीं देता। तो वह तमस् (अन्धकार) रूप होगा।" उत्तर है-"नहीं, ऐसा असम्भव है।"
"तो क्या?" "वह प्रकाशों का प्रकाश है" "ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ।"
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ।।१७ ।।
शब्दार्थ : ज्योतिषाम् - ज्योतियों का, अपि-भी, तत्-वह, ज्योति- ज्योति, तमसः - अन्धकार से, परम् -परे, उच्यते-कहा जाता है, ज्ञानम् - ज्ञान, ज्ञेयम् - ज्ञेय (जानने योग्य), ज्ञानगम्यम् - ज्ञान द्वारा प्राप्य, हृदि-हृदय में, सर्वस्य-सब के, विष्ठितम् - प्रतिष्ठित, स्थित ।
अनुवाद : ज्योतियों का भी ज्योति वह परमात्मा तमस् (अन्धकार) में से कहा जाता है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञेय और ज्ञान का लक्ष्य वह परब्रह्म सब के हृदयों में प्रतिष्ठित है।
व्याख्या : परमात्मा बुद्धि को प्रकाशित करता है, मन, सूर्य, चाँद, चितारे और अग्नि तथा विद्युत् को भी प्रकाश देने वाला वही है। वह स्वयं प्रभा है।
"वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न ही विद्युत् चमकती है, फिर इस लौकिक अग्नि का तो कहना ही क्या? उसके प्रकाशमान होते हुए सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है।" (कठोपनिषद् -२.२.१५ ; श्वेताश्वतरोपनिषद् -६.१४)
ज्ञान-नम्रता आदि (निरूपण –XIII.7 से 10)
ज्ञेय-जानने योग्य (इसी अध्याय के १२-१७ में देखें)
ज्ञानगम्य-ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य ।
प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि में ये तीनों स्थित हैं। यद्यपि सूर्य का प्रकाश सब पदार्थों में समान रूप से प्रकाशित होता है तथापि दर्पण आदि निर्मल तथा अधिक चमकीले पदार्थों में सूर्य की चमक बढ़ जाती है। इसी प्रकार ब्रह्म सब पदार्थों में विद्यमान होते हुए भी उसी से प्राप्त बुद्धि में वह विशेष आलोक से भासता है। (निरूपण-X.20; XIII.3; XVIII.61)
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ।।१८ ।।
शब्दार्थ : इति-इस प्रकार, क्षेत्रम् -क्षेत्र को, तथा-और, ज्ञानम् -ज्ञान, ज्ञेयम्-ज्ञेय, च-और, उक्तम्-कहे गये, समासतः संक्षेप में, मद्भक्तः- मेरा भक्त, एतत्-यह, विज्ञाय-जान कर, मद्भावाय-मेरे भाव को, उपपद्यते -प्राप्त करता है।
अनुवाद : इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है। इसे जान कर मेरा भक्त मेरे ही भाव को प्राप्त होता है।
व्याख्या : वह संयतेन्द्रिय, जिसे क्षेत्र और ज्ञेय का ज्ञान है और जो अपना चित्त मुझ में स्थिर करता है वह मुझे प्राप्त होता है।
इस प्रकार क्षेत्र, जिसका वर्णन महाभूतों से प्रारम्भ हो कर श्लोक ५ और ६ में 'दृढ़ता' पर समाप्त हुआ, ज्ञान का वर्णन ७ से ११ में 'अमानित्वम्' से प्रारम्भ हो कर 'यथार्थ दर्शनम्' में समाप्त हुआ और ज्ञेय विषय का वर्णन १२ से १७ में दिया गया-एवंविध ये तीन संक्षेप से निरूपित किये गये।
जिस व्यक्ति की मेरे प्रति अनन्य भक्ति की भावना है, जो मुझ को परम पुरुष, सर्वज्ञ और सर्वोच्च गुरु मानता है और सब को आत्म स्वरूप समझता है, जो वह मनन करता है, अनुभव करता है कि वह जो कुछ भी देख रहा है, सुन रहा है और स्पर्श कर रहा है वह सब भगवान् ही है अन्य कुछ नहीं और जो ऊपर बताये गये यथार्थ ज्ञान से युक्त है वह मेरे भाव को प्राप्त होता है अथवा आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है।
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि ।
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् । ।१९ ।।
शब्दार्थ : प्रकृतिम् -प्रकृति को, पुरुषम् -पुरुष को, च-और, एव-ही, विद्धि-जानो, अनादी -अनादि, उभौ दोनों, अपि-भी, विकारान् -विकारों को, च-और, गुणान् गुणों को, च-और, एव-ही, विद्धि-जानो, प्रकृतिसम्भवान् - प्रकृति से उत्पन्न ।
अनुवाद : प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि जानो और यह भी जान लो कि समस्त विकार और गुण प्रकृति से ही उद्भुत हैं।
व्याख्या : भवन की ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए सोपान अनिवार्य है। इसी प्रकार आत्म-ज्ञान के शिखर तक पहुँचने के लिए भी सोपान आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान् कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के सर्वोच्च शिखर तक ले जाने के लिए एक-एक चरण कर के आगे बढ़े। प्रथम तो भगवान् ने अर्जुन को क्षेत्र की प्रकृति से अवगत कराया, तदुपरान्त ज्ञान, अविद्या और अन्त में ज्ञेय का ज्ञान दिया। शिशु को भोजन कराने के लिए एक माँ भोजन को विभक्त कर के थोड़ा-थोड़ा खिलाती है। इसी प्रकार भगवान् ने अपने आध्यात्मिक शिशु को आध्यात्मिक भोजन थोड़ा-थोड़ा (अल्पशः) दिया।
भगवान् कृष्ण कहते हैं- "हे अर्जुन, यही उपदेश मैं तुम्हें प्रकृति और पुरुष के रूप में दूंगा।"
अब तक भगवान् ने उपनिषद् दर्शन के अनुरूप आत्मा और क्षेत्र का ज्ञान दिया। अब वही ज्ञान वे सांख्य दर्शन के अनुरूप देंगे किन्तु इसका वर्णन पुरुष और प्रकृति के मध्य भेद की द्वैत प्रकृति को अस्वीकारते हुए करेंगे।
विकार-महत्तत्त्व से ले कर शरीर पर्यन्त समस्त विकार अथवा परिणतियाँ, जो सांख्य दर्शन के २४ तत्त्वों के अन्तर्गत आती हैं। अन्तरात्मा अव्यय है। सभी परिवर्तन प्रकृति में होते हैं। मूल प्रकृति (आदि, अव्यक्त प्रकृति) महत्, अहंकार, महाभूत और अन्य अल्प विकारों को प्राप्त होती हैं।
जैसे बर्फ और शीतता, दिन और रात एक-दूसरे से अभिन्न हैं इसी प्रकार पुरुष और प्रकृति एक-दूसरे से पृथक् नहीं हैं। सत्त्व, रजस् और तमस्-ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। समस्त कर्म मन, प्राण, इन्द्रियाँ और भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं।
सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष न केवल नित्य और अनादि हैं प्रत्युत् एक-दूसरे से पृथक् हैं और स्वयं सृजित हैं। वेदान्त दर्शन के अनुसार प्रकृति अथवा माया ब्रह्म से उद्भूत है इसलिए न तो वह स्वयं सृजित है और न ही स्वतन्त्र है। माया पूर्ण रूप से ईश्वर के वशीभूत है। माया उसका कारण शरीर है। माया उसकी भ्रामक शक्ति है।
प्रकृति और पुरुष ईश्वर के स्वभाव हैं। इन दोनों को अनादि जानो । जिसका कोई प्रारम्भ नहीं, आदि नहीं वह अनादि है। क्यों कि ईश्वर नित्य है उसकी दो प्रकृतियाँ (प्रकृति और आत्मा) भी नित्य होनी चाहिए। (यह सांख्य दर्शन का मत है।)
ईश्वर इन दो प्रकृतियों (परा और अपरा प्रकृति) को धारण करने वाला है जिसके द्वारा सृष्टि का उद्भव, स्थिति और संहार होता है। इसीलिए वह स्वामित्व के गुणों से युक्त है और ब्रह्माण्ड पर राज्य करता है। इन प्रकृतियों का आदि नहीं है इसीलिए वे संसार का कारण हैं।
गौण प्रकृति (अपरा प्रकृति) अष्टधा है जिसका वर्णन अध्याय VII के श्लोक ४ में है और अब अध्याय XIII श्लोक १९ में वर्णित है। मुख्य प्रकृति अथवा परा प्रकृति जिसका वर्णन अध्याय VII के श्लोक ५ में आ चुका है वही परा प्रकृति अध्याय XIII के श्लोक १९ में पुरुष रूप में वर्णित है। यहाँ पुरुष का अभिप्राय जीवात्मा से है।
एक शिशु भी मुस्कराता है और आह्लादित होता है तथा शोक, भय, क्रोध, सुख, दुख अनुभव करता है। किसने सिखाया उसे? इस जन्म के शुभाशुभ कर्मों के संस्कार इनका कारण नहीं हो सकते। पूर्व जन्म के संस्कार ही इनका कारण हो सकते हैं। उन संस्कारों का कोई आधार भी होना चाहिए। इसी से जीवात्मा के पूर्व जन्म में अस्तित्व का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है और यह भी स्पष्ट है कि आत्मा अनादि है। यदि आप यह स्वीकार नहीं करते कि जीवात्मा अनादि है तो दो दोष समक्ष आते हैं, एक तो कृतनाश (किये कमाँ की फल-प्राप्ति न होना) और दूसरा अकृताभ्यागम (कारण रहित परिणाम)। शुभाशुभ कर्मों के परिणाम सुख और दुःख बिना अनुभव किए ही समाप्त हो जायेंगे। यह कृतनाश का दोष है। इसी प्रकार पहले न किये हुए शुभाशुभ कर्मों के परिणाम सुख और दुःख भी भोगने पड़ेंगे। वह अकृताभ्यागम के दोष हैं। इन दो दोषों का निवारण करने के लिए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवात्मा अनादि है। शास्त्र भी उच्च स्वर से घोष करते हैं कि आत्मा अनादि है।
कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।।२० ।।
शब्दार्थ : कार्यकारणकर्तृत्वे-कार्य और कारण को उत्पन्न करने में, हेतु-कारण, प्रकृति-प्रकृति, उच्यते-कही जाती है, पुरुष-पुरुष, सुखदु खानाम् -सुख-दुःख का, भोक्तृत्वे-भोगने में, हेतुः-कारण, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : कार्य और कारण को उत्पन्न करने में प्रकृति को हेतु माना जाता है और सुख-दुःख की अनुभूति में पुरुष को अर्थात् जीवात्मा को हेतु कहा जाता है।
व्याख्या : सुख और दुःख शुभ और अशुभ कर्मों के परिणाम हैं। इच्छाशक्ति मन को प्रेरित करती है और मन उस विषय की प्राप्ति हेतु इन्द्रियों को प्रेरित करता है। अच्छे और बुरे कर्म प्रकृति से प्रारम्भ होते हैं और सुख-दुःख का कारण बनते हैं। बुरे कर्म दुःख और शोक को जन्म देते हैं। अच्छे कर्म प्रसन्नता और सुख देने वाले होते हैं। आत्मा भोक्ता है। पत्नी कार्य करती है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है और पतिदेव उसके परिश्रम के फल का चुपचाप आनन्द लेता है। वह शान्त बैठ कर भोजन ग्रहण करता और मन की पूर्ण सन्तुष्टि करता है। इसी प्रकार प्रकृति कार्य करती है और जीवात्मा उसके परिणाम का फल सुख-दुःख रूप में भोगता है।
जब सत्त्व प्रधान हो तो अच्छे कर्म किये जाते हैं। रजस् प्रधान हो तो अच्छे-बुरे दोनों कर्म होते हैं। तमस् प्रधान होने पर पापिष्ठ, नियम विरुद्ध और अधर्म कर्म होते हैं। कहीं-कहीं कारण (cause) के स्थान पर करण (instrument) शब्द का प्रयोग हुआ है। करण के भाव में-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, बुद्धि, अहंकार और मन को करण माना गया है।
कार्य-परिणाम अर्थात् भौतिक शरीर । पंच महाभूत जो शरीर का निर्माण करते हैं, पाँच इन्द्रियाँ जो इन्द्रिय-विषयों का निर्माण करती हैं और जो प्रकृति से उत्पन्न हैं, 'कार्य' की श्रेणी में आते हैं। (ये हैं-आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) ये सब कार्य रूप हैं।
शरीर की रचना में, इन्द्रियाँ और उनकी संवेदनाओं में कारण रूप प्रकृति है। इस प्रकार संसार का कारण रूप प्रकृति है।
ईख कारण है, ईख का रस और शर्करा ईख के विकार हैं। दुग्ध कारण है। दही, मक्खन और घृत दुग्ध के विकार रूप हैं। जो भी किसी वस्तु विशेष का विकार होता है उसे कार्य की संज्ञा दी जाती है। जिससे विकार उत्पन्न होते हैं वह उनका कारण है। प्रकृति समस्त विकारों का स्रोत अथवा कारण है। वह हर वस्तु उत्पन्न करती है। दस इन्द्रियाँ, मन और इन्द्रियों के पाँच विषय अर्थात् पंच तन्मात्रायें-ये सब १६ विकृतियाँ अथवा कार्य हैं।
महत् (बुद्धि) मूल प्रकृति से उत्पन्न होती है। महत् से अहंकार की उत्पत्ति होती है। महत् मूल-प्रकृति का कार्य और अहंकार का कारण है। इस लिए महत् को प्रकृति-विकृति कहते हैं। महत्, अहंकार और पाँच तन्मात्रा-ये सात प्रकृति-विकृति हैं। इनमें से प्रत्येक अपने से पूर्व का विकार (कार्य) हैं। और अपर का कारण। पाँच तन्मात्रायें पाँच स्थूल भूतों को जन्म देती हैं। वे सूक्ष्म तत्त्व हैं। ये सात प्रकृति और विकृति दोनों हैं, कारण भी हैं और कार्य भी और 'कारण' के अन्तर्गत इनकी गणना की जाती है।
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण और शरीर की क्रियाओं का शुद्धात्मा पर अध्यास किया जाता है। इसीलिए अज्ञानी मनुष्य कहता है-मैं श्याम वर्ण हैं, मैं स्थूलकाय (मोटा) हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं अन्धा हूँ, मैं 'अमुक' का पुत्र हूँ, मैं जानता vec xi_{2} मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ आदि आदि।
चित्त अत्यन्त सूक्ष्म है और यह सूक्ष्म आत्मा के अत्यन्त निकट है। आत्मा की चेतना का चित्त में प्रतिबिम्ब पड़ता है चेतना का चिदाभास होने के कारण चित्त चेतना का अनुभव करता है और वृत्ति जाग्रत होती है- "मैं चैतन्य हूँ, शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ। मैं सुख-दुःख का अनुभव करता हूँ।" शुद्ध आत्मा के गुण चित्त पर आरोपित हो जाते हैं। प्रकृति और पुरुष में तथा चित्त और आत्मा में परस्पर अध्यारोपण होता है अर्थात् चित्त की चेतना उसमें चेतन पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ने से है। जब चित्त में बाह्य वस्तुएँ और चेतन पुरुष- इन दोनों का प्रतिबिम्ब पड़ता है उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप सा भासता है। यही संसार का कारण है।
पुरुष, जीव, क्षेत्रज्ञ और भोक्ता सब पर्यायवाची शब्द हैं। पुरुष, जिसका वर्णन यहाँ है, वह परमात्मा नहीं है। वह बद्ध-आत्मा है, वह आत्मा जो सुख - दुख भोगने और जन्म-मरण के लिए बाध्य है, विवश है। परमात्मा तो संसार से सदा मुक्त और निर्विकार है।
प्रकृति और पुरुष संसार का कारण हैं। प्रकृति से शरीर, मन, इन्द्रिय, प्राण और बुद्धि का उद्भव होता है। आत्मा सुख-दुःख भोगता है। संसार ही दुःख-सुख का अनुभव है। आत्मा संसारी है। वह सुख-दुःख की अनुभूति लेता है। (निरूपण-XV.9)
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।।२१ ।।
शब्दार्थ : पुरुषः पुरुष, प्रकृतिस्थः -प्रकृति में स्थित, हि-निश्चित रूप से, भुङ्क्ते-भोग करता है, प्रकृतिजान् -प्रकृति से उत्पन्न, गुणान् गुणों को, कारणम् कारावया मैं जब गुणों में अनुराण, अस्य- इसकी, सदसद्योनिजन्मसुको, शुभ-अशुभ जन्म।
अनुवाद : प्रकृति में स्थित पुरुष ही निश्चित रूप से प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। इन गुणों में अनुराग (आसक्ति) ही अच्छी-बुरी यौनियों में जन्म लेने का कारण है।
व्याख्या : प्रकृति में स्थित जीवात्मा, प्रकृति के गुणों द्वारा कर्मशील होता है और सुख, दुःख, भ्रान्ति का अनुभव करता है। वह सोचता है- ''मैं प्रसन्न हूँ। मैं शोकग्रस्त हूँ। मैं भ्रम में हूँ। मैं बुद्धिमान् हूँ।" इस प्रकार वह स्वयं को गुणों के साथ तद्रूप कर लेता है, व्यक्ति भाव को प्राप्त होता है तथा पवित्र, अपवित्र योनियों में जन्म लेता है। शरीर, मन और इन्द्रियों के माध्यम से जीवात्मा विषयों को भोग कर भोक्ता बन जाता है। ब्रह्म मौन साक्षी है और अभोक्ता है। सुख, दुःख, भ्रान्ति आदि गुणों से जीवात्मा की आसक्ति ही इसके जन्म का मुख्य कारण है। यदि श्लोक के उत्तरार्द्ध में संसार शब्द को रख दिया जाये तो अर्थ होगा-गुणों में आसक्ति ही अच्छी-बुरी योनियों में जन्म का कारण है और इसी से संसार का अस्तित्व है।
सत् योनि अथवा अच्छी योनि देवता आदि की है। असत् योनि अथवा बुरी योनि निकृष्ट पशु आदि की है। मानव योनि मिश्रित कर्मों के कारण सत् भी है और असत् भी अर्थात् अच्छी भी है और बुरी भी है।
पुरुषः प्रकृतिस्थः जीवात्मा जो प्रकृति में स्थित है। यह अविद्या है। प्रकृति के गुणों में आसक्ति काम है। अविद्या और काम संसार का कारण हैं।
ज्ञान और वैराग्य अविद्या और काम को नष्ट करते हैं। (निरूपण -XIV.5; XV.7)
उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ।।२२ ।।
शब्दार्थ : उपद्रष्टा साक्षी (द्रष्टा), अनुमन्ता-अनुमति देने वाला, चऔर, भर्ता-पालन करने वाला, भोक्ता-भोग करने वाला, महेश्वरः- महेश्वर, परमात्मा-परमात्मा, इति-इस प्रकार, च-और, अपि-भी, उक्तः-कहा जाता है, देहे देह में, अस्मिन्-इस, पुरुषः-पुरुष, परः परम।
अनुवाद : इस शरीर में स्थित परम पुरुष साक्षी द्रष्टा, अनुमन्ता (अनुमति देने वाला अथवा सन्मति देने वाला), भर्ता (पोषक), भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा नाम से अभिहित है।
व्याख्या : उपद्रष्टा द्रष्टा, साक्षी, देखने वाला, किनारे खड़ा हुआ, पास बैठा हुआ। यज्ञिय अनुष्ठान करने के लिए जब पुरोहित और यजमान आसन ग्रहण करते हैं तो एक अनुभवी विद्वान् भी उनके समीप आसनस्थ होता है जिसे इन क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान और अनुभव होता है। वह यज्ञ में भाग नहीं लेता प्रत्युत् मौन द्रष्टा बन कर बैठता है। आवश्यकता पड़ने पर वह उनका पथ-प्रदर्शन करता है। उनके दोष दूर कर के उन्हें उचित बात कहता है। इसी प्रकार परमात्मा क्रिया नहीं करता। मन, बुद्धि, शरीर की क्रियाओं में वह भाग नहीं लेता । वह उनसे सर्वथा पृथक् है। वह उनकी क्रियाओं का मौन साक्षी है। वह प्रकृति के समीप रहता है और उसके क्रिया कलापों पर दृष्टि रखता है।
इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से भी की जा सकती है। शरीर, नेत्र, मन, बुद्धि और आत्मा द्रष्टा हैं। इनमें शरीर सर्वाधिक बाह्य द्रष्टा है जबकि आत्मा सर्वाधिक अन्तस्तम और निकटतम द्रष्टा है। आत्मा से परे अन्य कोई अन्तर्द्रष्टश नहीं है।
अनुमन्ता-अनुमति देने वाला। परमात्मा संमति देता है। यह इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि द्वारा कृत कर्मों को अनुज्ञा अथवा सन्तुष्टि प्रदान करता है। राजा की अनुमति मिलने पर प्राइम मिनिस्टर (मुख्य मंत्री) और अन्य आफिसर (कार्यकर्ता) कार्य करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज्ञा देता है और इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि अपने-अपने कार्य करते हैं। प्रतीति तो यह होती है कि वह परम पुरुष भी कार्य रत है अथवा उनकी सहायता में लगा है किन्तु क्योंकि वह तो केवल साक्षी द्रष्टा है अतः इन्द्रिय-मन-बुद्धि के कार्यों में नहीं आता।
भर्ता-पोषक । पति जिस प्रकार अपनी पत्नी को सहारा देता है उसी प्रकार शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों को आत्मा सहारा देता है, यह उनसे पृथक् है उसी प्रकार जैसे पिता अपने बच्चों का पालन करता है और उनसे पृथक् है।
भोक्ता-भोग करने वाला । आत्मा जो शाश्वत और चैतन्य स्वरूप है। उष्णता जिस प्रकार अग्नि का नैसर्गिक गुण है उसी प्रकार नित्य चैतन्यता आत्मा का समवायी गुण है। मन की समस्त अवस्थायें-सुख दुःख, भ्रम आदि चेतन आत्मा से आच्छादित और ज्योतित रहती हैं। जिस प्रकार भोजन ग्रहण करने वाला गोविन्दन भोजन से पृथक् है उसी प्रकार आत्मा, इन्द्रिय, मन और बुद्धि से पृथक् है किन्तु सुख-दुःख आदि प्रतीतियों से ग्रस्त हुआ सा प्रतीत होने के कारण चेतन आत्मा को भोक्ता कहा जाता है।
महेश्वर-महान् प्रभु । सब का आत्मा, सार तत्त्व और सब से स्वतन्त्र होने से वह महेश्वर है। आकाश बहुत विशाल है। महेश्वर आकाश से भी विशाल है और इसीलिए महेश्वर अभिहित है। जिस प्रकार सम्राट अपनी प्रजा से पृथक् होता है उसी प्रकार आत्मा प्रकृति, उसके कार्यों और विकारों से सर्वथा पृथक् है।
परमात्मा-वह परम है क्योंकि अव्यक्त से लेकर भौतिक शरीर पर्यन्त समस्त वस्तुओं में श्रेष्ठ है जिसमें अज्ञानवश आत्मा का अध्यारोपण किया जाता है। चुम्बक के समक्ष लौह खण्ड की भाँति परमात्मा की विद्यमानता में मन और बुद्धि जड़ होते हुए भी गति करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे चन्द्रमा अपना प्रकाश सूर्य से लेता है उसकी प्रकार मन और बुद्धि परमात्मा से प्रकाश ग्रहण करते हैं। परमात्मा स्वयं प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है, मन और बुद्धि में अपना प्रकाश नहीं है। वेदों में भी उसे परमात्मा कहा गया है। अध्याय XV के श्लोक १७ में भगवान् कृष्ण कहते हैं- “किन्तु उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा जाता है” “तुम भी मुझे सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जानो।" ऐसा भगवान् ने विस्तार से उपदेश दिया है और यह विषय यहाँ समाप्त होता है।
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ।। २३ ।।
शब्दार्थ: य-जो, एवम् इस प्रकार, वेत्ति-जानता है, पुरुषम् -पुरुष को, प्रकृतिम् -प्रकृति को, च-और, गुणै:-गुणों के, सह-साथ, सर्वथा-सब प्रकार से, वर्तमान रहता हुआ, अपि-भी, न-नहीं, स-वह, भूय-पुन, अभिजायते जन्म लेता है।
अनुवाद : जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष और गुणों सहित प्रकृति को जान लेता है वह कैसी भी अवस्था में रहे, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
व्याख्या : गुणों सहित प्रकृति को और पुरुष को जानने वाला स्वयं को जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त कर लेता है। चाहे वह जीवन की किसी भी अवस्था में कोई भी कार्य क्यों न करता हो । प्रकृति और पुरुष के विवेकपूर्ण ज्ञान का यही लाभ है। वह जानता है कि 'वह' नित्य है, अपरिवर्तनशील है और जो भी परिवर्तन होते हैं वे सब प्रकृति के गुणों की विकृति के कारण होते हैं। आत्मा शरीर के साथ एकत्व स्थापित कर के अविद्या के कारण दुःखी होता है और पुनर्जन्म के भंवर में फंस जाता है।
वह किसी भी अवस्था में हो, किसी भी कार्य में नियुक्त हो-वे चाहे कर्तव्य कर्म हों अथवा निषिद्ध कर्म, (जैसे इन्द्र ने पुरोहित विश्वरूप और अनेक संन्यासियों की हिंसा की), वह पुनः जन्म नहीं लेता क्योंकि पुनर्जन्म के बीज रूप कर्म आत्म-ज्ञान से, पुरुष-प्रकृति के ज्ञान से दग्ध हो चुके हैं, ज्ञानाग्नि ने उन कर्मों को भस्म कर दिया है। जिस प्रकार अग्नि में जले हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते उसी प्रकार ज्ञानाग्नि में भस्मीभूत कर्म पुनः जन्म अथवा शरीर प्रदान करने में शक्य नहीं होते। इस अवस्था में उनकी स्थिति कर्माभास की होती है। वे प्रभावपूर्ण कारण नहीं हैं और नया जन्म नहीं दे सकते। एक जला हुआ वस्त्र, वस्त्र का कार्य नहीं कर सकता।
फल की इच्छा से और अहंकारवश किये गये कर्म परिणामदायी होंगे। एक विद्वान पुरुष अविद्या, अहंकार और आसक्ति के बीजों को ज्ञानाग्नि में भस्म कर देता है। इसीलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता ।
वर्तमान को जन्म दे कर जिन प्रारब्ध कर्मों ने अपना व्यापार पहले ही प्रारम्भ कर दिया है, वे नष्ट नहीं होते भले ही आत्मा के ज्ञान का सूर्य उदय हो आशाये । तरकस से निकाल कर एक बाण जो लक्ष्य पर छोड़ा गया है। वह लक्ष्य अदन करने के उपरान्त भी शक्ति समाप्त होने और घरा पर गिरने पर्यन्त भोरयाशील रहता है। इसी भाँति शरीर को स्वरूप देने वाले प्रारब्ध कर्म तब तक कार्यरत रहते हैं जब तक समवाय शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाती, इसी शरीर के माध्यम से ही चाहे विद्वान् पुरुष ने आत्म-ज्ञान क्यों न प्राप्त कर लिया हो, प्रारब्ध कर्म का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। किन्तु अवधारणा के योग्य तथ्य तो यह है वह विद्वान् पुरुष इससे किंचित् मात्र भी प्रभावित नहीं होता क्यों कि उसने देह के साथ एकत्व स्थापित नहीं किया है, वह तो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया है। शरीर में यदि कैंसर का व्रण भी हो जाये प्रारब्ध कर्मों के कारण, तो भी वह कदापि व्याकुल नहीं होगा क्योंकि वह देह-चेतना से ऊपर उठ चुका है और साक्षी बन कर स्वयं अपनी देह को देख रहा है। किन्तु कोई देखने वाला राहगीर यह दोषपूर्ण कल्पना करेगा कि मुक्त संन्यासी भी सामान्य मनुष्य की भाँति दुःख भोग रहा है। यह गम्भीर और कष्टप्रद भूल है। मुक्तात्मा के विचार में न तो शरीर है और न ही प्रारब्ध कर्म है।
धनुष पर साधा हुआ बाण, जो अभी छोड़ा नहीं गया, वापस लिया जा सकता है, उसका प्रतिसंहरण हो सकता है। इसी प्रकार जिन कर्मों का परिणाम अथवा प्रभाव अभी प्रारम्भ नहीं हुआ, वे आत्म ज्ञान द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं। अतः यह कहना उचित ही है कि मोक्ष प्राप्ति के पश्चात् जन्म नहीं होता। जिस शरीर से आप्तकाम पुरुष ने आत्म-ज्ञान प्राप्त किया वह नष्ट होने पर पुनः शरीर धारण नहीं करता । इस शरीर का कारण अविद्या जब आत्म-ज्ञान से दूर हो जाती है तो अविद्या का प्रभाव-दूसरा जन्म-वह भी नष्ट हो जाता है। साधारण मनुष्य जैसे शुभाशुभ कर्मों के कारण जन्म लेता है एक विद्वान् पुरुष ऐसे जन्म नहीं लेगा क्योंकि आत्म-ज्ञान से उसके समस्त संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। आत्म-ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् किये जा रहे उसके कर्म उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते क्योंकि वह इच्छा मुक्त और अहंकार शून्य हो चुका है। (निरूपण-XIII.32)
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।।२४ ।।
शब्दार्थ : ध्यानेन-ध्यान के द्वारा, आत्मनि-आत्मा में, पश्यन्ति - देखते हैं, केचित् कुछ, आत्मानम्-आत्मा को, आत्मना-आत्मा के द्वारा, अन्ये-अन्य, सांख्येन योगेन-सांख्य योग (ज्ञान योग) के द्वारा, कर्मयोगेन कर्मयोग के द्वारा, च-और, अपरे अन्य ।
अनुवाद : आत्मा में, आत्मा को, आत्मा के द्वारा कुछ (साधक) ध्यानयोग से देखते हैं, कुछ ज्ञान योग से और अन्य कर्मयोग से देखते हैं।
व्याख्या : प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान-प्राप्ति के अनेक पथ हैं। प्रथम तो महर्षि पतञ्जलि का ध्यान योग का मार्ग है। राजयोगी आत्मा को (सूक्ष्म, तत्त्वदर्शी) बुद्धि से परिमार्जित हृदय में देखते हैं। तैलधारावत्, ध्यान, आत्म-सम्बद्ध विचारों का अनवरत, अखण्ड प्रवाह है। ध्यान (एकाग्रता) के द्वारा कर्ण आदि इन्द्रियों को हृदय में संहत किया जाता है। इन्द्रियों को उनके विषयों की ओर भागने से रोका जाता है। संहरण (प्रत्याहार) की प्रक्रिया से उन्हें पूर्णतया वश में रखा जाता है, संयत किया जाता है। तत्पश्चात् मन को ही आत्मा में सतत ध्यान के द्वारा आत्मा में प्रतिष्ठित किया जाता है। ध्यान से ही मन शुद्ध पवित्र होता है। शुद्ध मन स्वभावतः आत्मा की ओर उन्मुख होगा। इन्द्रिय-विषयों से न तो यह आकृष्ट होता है और ही उनमें आसक्त होता है।
सांख्य योग-यह ज्ञान योग है। साधक विचारणा और आत्म विश्लेषण के द्वारा स्वयं को प्रकृति के तीन गुणों से तीन शरीरों और पंच कोषों से पृथक् कर के साक्षी परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करता है। वह विचार करता और अनुभव भी करता है कि वह तीन गुणों से अतीत है, मौन साक्षी है, अनासक्त है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अमर है, अनश्वर है, स्वयंभू है, स्वयंप्रभा है, अखण्ड है, अजन्मा और अव्यय है।
कर्मयोगी अपने कर्म और उनका फल प्रभु को समर्पित कर देता है। उसकी बुद्धि ईश्वरार्पण भाव से युक्त होती है। इस भाव से मन में शुद्धता आती है और ज्ञानोदय होता है। मन की पवित्रता से कर्मयोग में, मन की एकाग्रता का विकास होता है। इसी पवित्रीकरण से मन आत्मा-परमात्मा के योग की ओर अग्रसर होता है इसीलिए इसे (कर्म को) भी योग की संज्ञा दी गई है।
सांख्य योग का अभ्यास करने वाले साधक सर्वोच्च श्रेणी के हैं। ध्यान योग का अनुसरण करने वाले आध्यात्मिक साधक मध्यम श्रेणी के हैं और कर्मयोग का अभ्यास करने वाले निम्नतम श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास और कठोर साधना के द्वारा निम्न और मध्यम श्रेणी के साधक शीघ्र ही उत्तम श्रेणी में आ जाते 51 (f7849-V.5;V1.46)
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते ।
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ।।२५ ।।
शब्दार्थ : अन्ये-अन्य, तु-निश्चयेन, एवम् - इस प्रकार, अजानन्तःन जानते हुए, श्रुत्वा सुन कर, अन्येभ्यः दूसरों से, उपासते-उपासना करते हैं, ते-वे, अपि भी, च और, अतितरन्ति-तर जाते हैं, एव-ही, मृत्युम् -मृत्यु को, श्रुतिपरायणा श्रुतिपरायण ।
अनुवाद : अन्य लोग भी इस का (योग का) ज्ञान न स्खाते हुए दूसरों से श्रवण कर के उपासना करते हैं और वे श्रुतिपरायण लोग परमात्मा की शरण लेकर इस मर्त्य लोक hat H तर जाते हैं।
व्याख्या : ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्मयोग-ये तीन मार्ग ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व श्लोक में बताये गये हैं। इस श्लोक में उपासना योग का उपदेश दिया जा रहा है।
पूर्व श्लोक में वर्णित विधियों से अनभिज्ञ लोग आध्यात्मिक गुरुजनों और विद्वानों से उस महान् सत्य स्वरूप परमात्मा के विषय में पूर्ण निष्ठा और अविचल श्रद्धा से उपदेश श्रवण करते हैं। वे पूर्णतया दूसरों के आधिकारिक उपदेश पर निर्भर करते हुए सतत स्मरण (जप) और ध्यान के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। वे अपने गुरु के प्रति भक्तिभाव रखते हैं। कुछ साधक साक्षात्कार प्राप्त ऋषियों के ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं, उनमें लिखित उपदेशों को निष्ठापूर्वक ग्रहण कर के उनके अनुरूप जीवन यापन करते हैं। वे भी मृत्यु से तर जाते हैं। कोई किसी भी मार्ग का अनुसरण करे, अन्ततः आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर के जन्म-मृत्यु से तर कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। विभिन्न साधन युक्त और विभिन्न स्वभाव वालों के लिए उनके अनुरूप विभिन्न मार्ग हैं।
आत्म-ज्ञान से अपने अज्ञान और उसके प्रभावों से स्वयं को मुक्त करना संसार सागर से तरना है। यही अमृतत्व है, यही निर्वाण है, यही मृत्यु से तरना है।
यावत्सञ्जायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ।। २६ ।।
शब्दार्थ : यावत् जो भी, सञ्जायते-उत्पन्न होता है, किंचित् -कुछ भी, सत्त्वम् सत्त्व (अस्तित्व), स्थावरजङ्गमम् -चर और अचर, क्षेत्रक्षेत्रसंयोगात् -क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, तत्-वह, विद्धि-जानो, भरतर्षभ - हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ (अर्जुन)।
अनुवाद : हे अर्जुन, इस बात को जान लो कि स्थावर अथवा जङ्गम कोई भी वस्तु कहीं भी उत्पन्न हुई है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुई है।
व्याख्या : हे अर्जुन, संसार में स्थावर-जङ्गम जो भी पदार्थ हैं उन्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग vec H उत्पन्न जानो ।
क्षेत्र को जानने वाले (क्षेत्रज्ञ) आकाश की भाँति अखण्ड हैं। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग दो खण्डों के सम्पर्क से नहीं हो सकता जैसे ड्रम और स्टिक, रज्जु और पात्र आदि । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परस्पर सम्बन्ध कारण और कार्य का भी नहीं है जैसे सिर और ग्रीवा, भुजा और कन्धा-इनका परस्पर संयोग अविभाज्य है पुनरपि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग इन सब से परे है, अतीत है, विलक्षण है, अलौकिक है।
तो फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग किस प्रकार का है? यह संयोग एक मेरे पर अध्यारोपण का है अध्यास का है, भ्रम का है। यह गुणों सहित एक का बरे में भ्रान्ति का संयोग है। रज्जु और सर्प, मुक्ता- शुक्ति (मोती बनाने वाली अप) और चाँदी में विवेक के अभाव में भ्रम हो जाता है अर्थात् भ्रमवश मनुष्य अंधेरे में रज्जु को साँप समझ बैठता है और डर जाता है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में उसे सीप में चाँदी का भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा के गुणों का, अज्ञानी मनुष्य, शरीर में अध्यास कर लेता है अर्थात् शरीर को ही आत्मा मानने लगता है। जड़ शरीर को भ्रान्ति के कारण चेतन आत्मा मान कर प्रकृति के शरीर की क्रियाओं को मौन निष्क्रिय आत्मा में निक्षिप्त करता है। इस प्रकार के भ्रम का निराकरण हो जाये यदि साधक आत्म-ज्ञान प्राप्त कर ले, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त कर ले, उन दोनों का भेद जान ले और वह क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र को पृथक् करने में इतना प्रवीण हो जाये जैसे मुंज में से सींक को मुंज घास से अलग किया जाता है। जब वह जान लेता है कि ब्रह्म सब सीमित उपाधियों से उसका अपना ही आत्म तत्त्व है और आभास मात्र है, वह सीप में चाँदी की भाँति (आभास) है। वह आक्त क्षेत्र तो व्पनिक भवन (हवाई किला) है अथवा नगर है, स्वप्न में देखे गये दृश्य की शांति है अथवा एक जादूगर के द्वारा बनाये गये घोड़े, स्थान और वन आद की भाँति है। ये समस्त भ्रान्तियाँ दूर हो जायें और आत्म-ज्ञान हो जादे की जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति मिलती है।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।।२७ ।।
शब्दार्थ : समम् -सम, सर्वेषु सब (में), भूतेषु-भूतों (प्राणियों) में, तिष्ठन्तम्-स्थित, निवास करते हुए, परमेश्वरम् -परमेश्वर को, विनश्यत्सु - विनाशशील में, अविनश्यन्तम् - अविनाशी को, यः- जो, पश्यति-देखता है, सः- वह, पश्यति-देखता है।
अनुवाद : जो मनुष्य परमेश्वर को सब भूतों में समभाव से स्थित और विनाशशील जगत् में उस अविनाशी को देखता है, वही यथार्थ देखता है।
व्याख्या : जो परमात्मा को ज्ञान-चक्षु से, ब्रह्मा से ले कर जीव जगत् के समस्त प्राणियों में निवसित देखता है और नश्वर पदार्थों के नष्ट होते हुए भी उनमें स्थित उस अविनाशी परमात्मा के दर्शन करता है वह आत्म-ज्ञानी कहलाता है।
विभिन्न प्रकार की अग्नियों में उष्णता एक है। आभूषणों की विभिन्नता में स्वर्ण एक है। पृथक् पृथक् दीपों से प्रकाश एक ही है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों में आत्मा एक है। आत्मा सर्वत्र समरूप है। चींटी, हाथी, राजा, भिखारी, सन्त, और डाकू सब में आत्मा एक है।
आत्मा का विनाश नहीं होता। सब जीव जगत् के प्राणी विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति और जीवात्मा-तुलना की जाये तो एक परमेश्वर ही है जिसकी यह सब माया है।
परिवर्तन, विकास, हास और मृत्यु आदि भाव-विकारों का मूल कारण जन्म है।
परमात्मा एक है, अविकारी है, अजन्मा है, अव्यय है और अमृत स्वरूप है। वह समस्त प्राणियों में एक चेतन है। वह यथार्थ देखता है जो इस प्रकार से वर्णित परमेश्वर को देखता है। वह जीवन्मुक्त है। उसे क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, अमृत स्वरूप परमात्मा का ज्ञान है। वह वास्तविक द्रष्टा अथवा मुक्तात्मा है।
ज्ञानी ही वस्तुतः देखता है क्योंकि वह ज्ञान से युक्त है। सारा संसार अज्ञान वश मिथ्या दर्शन ही करता है। जिसके नेत्र तिमिर रोग से दूषित हों उसे अनेक चन्द्र दिखाई देंगे। वह गलत (अयथार्थ) देखता है। किन्तु एक ही चन्द्र को देखने वाला सही (यथार्थ) देखता है। इसी प्रकार जो अमर, अखण्ड एक परमात्मा को सब प्राणियों में देखता है वह सत्य देखता है। केवल वही देखता है। अन्य लोग तो देखते हुए भी नहीं देखते। उनकी दृष्टि तो अनेक चन्द्रमा के दर्शन करने वाले की भाँति है। (निरूपण-VIII.20)
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।
न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम् ।।२८ ।।
शब्दार्थ : समम् -सम, पश्यन्-देखते हुए, हि-वस्तुतः, सर्वत्र सर्वत्र, समवस्थितम् -समान रूप से विद्यमान, ईश्वरम्-ईश्वर को, न-नहीं, हिनस्ति-चोट पहुँचाता है, आत्मना आत्मा से, आत्मानम्-आत्मा को, ततः-तब, याति-जाता है, पराम् - उत्कृष्ट, सर्वोच्च, गतिम् - गति को ।
अनुवाद : क्योंकि जो मनुष्य परमेश्वर को सर्वत्र समान रूप से विद्यमान देखता है वह आत्मा से आत्मा का हनन नहीं करता, वह सर्वोच्च पद (लक्ष्य), उत्तम गति को प्राप्त करता है।
व्याख्या : यह आत्म-ज्ञान की दृष्टि है। परमेश्वर सब रूपों में विद्यमान है। उससे पृथक् कुछ नहीं।
एक अज्ञानी पुरुष अपनी देह, मनोविकारों को ही आत्मा मान कर और सब प्राणियों में एक परमात्मा के दर्शन न कर के, अपनी ही आत्मा को नष्ट करता है क्योंकि वह भ्रम जाल में फंसा हुआ है। उसकी दृष्टि दूषित है। उसका मन अत्यन्त स्थूल है। वह सूक्ष्म आत्मा का चिन्तन भी नहीं कर सकता। वह अज्ञान के वशीभूत है। अपवित्र शरीर में वह पवित्र आत्मा का अध्यास करता है। उसका ज्ञान अयथार्थ है, विवेक शून्य है। किन्तु ज्ञानी को आत्मा का ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है और वह सर्वत्र एक ईश्वर के दर्शन करता है।
अज्ञानी तो अपनी ही आत्मा का हनन करने वाला है। एक शरीर के नष्ट होने पर वह और-और शरीर धारण करता रहता है। समद्रष्टा, आत्मा से आत्मा का करता। इसीलिए वह परम लक्ष्य, प्राप्ति करता है। आत्मा का ज्ञान मोक्षदायक है। परमात्मा का ज्ञान अमोल की पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। अज्ञान और मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जायें तो सभी बुराइयाँ स्वतः ही नष्ट हो जायें।
सब भूतों में एकत्वदर्शी कभी आवागमन के चक्र में नहीं फंसते । वे तुर्यावस्था को प्राप्त होते हैं जो जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था से अन्य चतुर्थ अवस्था है और जहाँ शब्द और रूप का अस्तित्व नहीं है। आत्मा ही सबका मित्र (बन्धु) है और आत्मा ही शत्रु भी है। यह भाव पहले अध्याय VI के श्लोक ५,६ में आया है और यहाँ पुनरुक्ति हुई है। (निरूपण-XVIII.20)
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ।। २९ ।।
शब्दार्थ : प्रकृत्या-प्रकृति के द्वारा, एव-ही, च-और, कर्माणि-कर्म, क्रियमाणानि-किये जा रहे, सर्वशः सब, यः-जो, पश्यति-देखता है, तथा-वैसे ही, आत्मानम्-आत्मा को, अकर्तारम्-अकर्ता, सः- वह, पश्यति-देखता है।
अनुवाद : वही देखता है जो यह देखता है कि समस्त कर्म पूर्ण रूप से प्रकृति के द्वारा किये जा रहे हैं और आत्मा अकर्ता है।
व्याख्या : समस्त चेष्टाओं के लिए प्रकृति उत्तरदायी है। आत्मा कर्म से अतीत है। यह केवल साक्षी द्रष्टा है। ऐसा अनुभव करने वाला यथार्थतः ज्ञानी है।
जो यह जान लेता है कि सारे कर्म जो कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों तथा मन-बुद्धि से सम्पन्न हो रहे हैं उनमें प्रकृति हेतु है और आत्मा अकर्ता है, वह वास्तव में देखता है। केवल वही देखता है। जो व्यक्ति मूढ़ता वश इन्द्रिय-मन-बुद्धि से एकीभाव कर लेता है और आत्मा को कर्ता मानता है वह व्यक्ति अविद्या में पड़ा हुआ है। वह केवल चर्म चक्षुओं से देखता है। उसके पास दिव्य ज्ञान का अन्तर्चक्षु नहीं है। आकाश निष्क्रिय रहता है किन्तु मेघ आकाश में गति करते हैं। इसी प्रकार आत्मा अकर्ता है किन्तु प्रकृति सब कुछ करती है। आत्मा में कोई सीमित प्रतिबन्धक नहीं है। आकाश में जैसे कोई विभिन्नता नहीं है वैसे ही आत्मा एक है उसमें कोई विभिन्नता नहीं है। यह अद्वितीय समभाव रूपी सार तत्त्व है। यह किसी भी प्रकार के गुण, विशेषण, लक्षण से अतीत है। (निरूपण - III.27, XIV.19, XVIII.16)
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।।३० ।।
शब्दार्थ : यदा-जब, भूतपृथग्भावम् - भूतों का पृथक्ता का भाव, एकस्थम् - एक में स्थित, अनुपश्यति-देखता है, तत-वहाँ से, एव-ही, च-और, विस्तारम् विस्तार को, ब्रह्म-ब्रह्म, सम्पद्यते (वह) हो जाता है, तदा तब ।
अनुवाद : जिस समय मनुष्य प्राणियों के पार्थक्य भाव को एक में स्थित और उसी से विस्तार को प्राप्त होते हुए देखता है तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है।
व्याख्या : अलौकिक ज्ञान द्वारा अनेक में एक को देखने वाला मनुष्य परब्रह्म से एकीभाव को प्राप्त होता है। जल में ऊर्मियाँ, पृथ्वी में अणु, सूर्य में किरणें, शरीर में अवयव (अङ्ग), मन में विचार, अग्नि में प्रस्फुल्लिंग (चिंगारियाँ) की भाँति निश्चित रूप से समस्त रूप उस एक परमात्मा में बद्ध-मूल हैं। जब भी वह अपनी दृष्टि परावृत करता है वह एक परमात्मा का ही दर्शन करता है और आनन्द में रहता है।
जब वह भूतों की विभिन्नता गुरु और शास्त्रोपदेश के अनुरूप एक में बद्धमूल देखता है तब वह आत्म-ज्ञान की अनुभूति से जान जाता है कि जो कुछ भी देख रहा है वह केवल आत्मा ही है इससे अन्य कुछ नहीं और उद्भव एवं विस्तार केवल उसी एक (अद्वितीय) से है। छान्दोग्योपनिषद् ७.२६.१ में यही भाव एवंविध वर्णित है -
आत्मतः प्राण आत्मत आशा आत्मतः स्मर
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आपः
आत्मत आविर्भावतिरोभावावात्मतोऽन्नम् ।।
"(इस प्रकार देखने वाले विद्वान के लिए) आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जाये आशाला से आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मा से अन्न-यह सब हो जातो जल,
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।।३१ ।।
शब्दार्थ : अनादित्वात्-अनादि होने से, निर्गुणत्वात् -निर्गुण होने से. अयम कान्यह, अव्यय: अविनाशी, शरीरस्थ: हीरो यानि लिम होता हे। है कुन्ती पुत्र, न-नहीं, करोति करता है, परमात्मा-परमात्मा, ३- नहीं, लिप्यते-लिप्त
अनुवाद : हे अर्जुन, परमात्मा अनादि, अव्यय और निर्गुण होने से सब प्राणियों में विद्यमान होते हुए भी न तो कर्म करता है और न ही उसमें लिप्त होता है।
व्याख्या : परमात्मा प्रकृति से परे है। इसलिए गुणों से अतीत है। निर्गुण है। प्रकृति में चेष्टा इसके अपने ही समवायी गुणों से है। परमात्मा इस जीवात्मा के शरीर से पूर्व भी था और इसके नष्ट होने के पश्चात् भी रहेगा। यह शाश्वत रूप से एक रस और अनश्वर है।
अव्ययः- आविर्भाव और तिरोभाव अथवा जन्म-मरण से जो अतीत है। जिसका आदि है उसका अन्त भी है। उद्भव के उपरान्त वस्तु में परिणति (विकास, क्षय आदि) आती है। आत्मा जन्मरहित होने से सब प्रकार के परिणामों (परिवर्तन) से मुक्त है अर्थात् इसमें उदय और क्षय (जन्म-मृत्यु) नहीं होता, वृद्धि और क्षय भी नहीं होता और यह 'अस्ति', 'भाति' के गुणों से भी अतीत है। सब प्रकार की प्रक्रियाओं से स्वतन्त्र है इसलिए यह अव्यय है। जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब भले ही गति करता हुआ दृष्टिगोचर हो किन्तु वास्तव में सूर्य गति नहीं करता। इसी प्रकार परब्रह्म कर्मफल से अस्पृष्ट रहता है क्योंकि यह कर्ता नहीं है, प्रकृति के गुणों से परिच्छिन्न भी नहीं है, अविभाज्य है, अखण्ड है, निष्क्रिय है, अनादि, अनासक्त और कारण रहित है।
परमात्मा तीन प्रकार के भेदों से अतीत है अर्थात् -सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। एक आम का वृक्ष खजूर के वृक्ष से पृथक् है, यह सजातीय भेद है। एक आम का वृक्ष पत्थर से पृथक् है, यह विजातीय भेद है। उसी आम के वृक्ष के पत्ते, फूल और फल पृथक् पृथक् हैं, यह स्वगत भेद है। किन्तु परमात्मा अद्वैत है। कोई और ब्रह्म उसके समान नहीं है। इसलिए ब्रह्म का सजातीय भेद नहीं हो सकता। यह संसार एक आभास (प्रतीति) है। यह हमारी कल्पना का भ्रम है। अज्ञानवश यह ब्रह्म पर अध्यासित है। काल्पनिक पदार्थ का, अपना आलम्बन छोड़ कर अन्य कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। जैसे रज्जु में सर्प का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, वह अपने आलम्बन रज्जु में प्रभासित हो रहा है। इसलिए ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं हो सकता। ब्रह्म अविभाज्य है, भाग रहित अव्यय है, गुणातीत है, रूप, रङ्ग, अङ्ग रहित है अतः ब्रह्म में स्वगत भेद भी असम्भव है।
ब्रह्म अनादि है। कारण रहित है। स्वयंभू है। खण्ड रहित है। गुण रहित है। उपाधि रहित है। अतः अमृत स्वरूप है। अनासक्त होने से न कर्ता है न भोक्ता है। ब्रह्म यदि कर्ता और भोक्ता है तो वह ब्रह्म नहीं है। किसी भी प्रकार से यह हम सब से सर्वश्रेष्ठ है। कर्तृत्वभाव और भोक्तृभाव अज्ञान वश अहंकार में आरोपित हैं। प्रकृति ही कार्य करती है अथवा गुण ही गुणों में बरतते हैं। (निरूपण-V.14, XV.9)
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।
सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ।। ३२ ।।
शब्दार्थ : यथा-जैसे, सर्वगतम् -सर्वव्याप्त, सौक्ष्म्यात् - सूक्ष्मता के कारण, आकाशम् आकाश, न-नहीं, उपलिप्यते-लिप्त होता है, सर्वत्र सर्वत्र, अवस्थित-स्थित, देहे-शरीर में, तथा-वैसे, आत्मा-आत्मा, ननहीं, उपलिप्यते-लिप्त होता है।
अनुवाद : सर्वव्यापक आकाश जिस प्रकार से सूक्ष्मता के गुण के कारण लिप्त नहीं होता उसी प्रकार आत्मा शरीर में सर्वत्र होते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता।
व्याख्या : आकाश सर्वत्र व्याप्त है। सर्वस्व इसी में विलीन होता है। ऐसा कोई केन्द्र-बिन्दु नहीं है जहाँ से आकाश झांकता न हो और जहाँ व्याप्त न हो पुनरपि यह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा सारे शरीर में और पूर्ण विश्व में व्याप्त है। शरीर से सूक्ष्म होने के कारण यह न तो शरीर से न ही किसी अन्य वस्तु से लिप्त होता है। यह अनासक्त और कर्मरहित है। इसके कोई भाग (खण्ड) नहीं, कोई अवयव नहीं। यह सदा पावन और निष्कलंक है।
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ।।३३ ।।
शब्दार्थ : यथा- जैसे, प्रकाशयति-प्रकाशित करता है, एक-एक, कृत्स्नम् -संपूर्ण, लोकम् लोक को, इमम् यह, रविः सूर्य, क्षेत्रम् एकः हो, क्षेत्री क्षेत्र का स्वामी, (परमात्मा), तथा वैसे ही, कृत्वनम् रामसेत करता है, भारत-हे' भरत वंशी (अर्जुन)। प्रकाशयति-प्रकाशित
अनुवाद : हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य समस्त ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार परमात्मा, क्षेत्र का स्वामी, सम्पूर्ण क्षेत्र (शरीर) को प्रकाशित करता है।
व्याख्या : परमात्मा एक है। अव्यक्त से लेकर तृण पर्यन्त, 'पंच महाभूतों' के मिट्टी के ढेले से लेकर 'सत्त्व' और धृति पर्यन्त सब पदार्थों (प्रकृति) को वह परमात्मा प्रकाशित करता है। जिस प्रकार सूर्य एक है, वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को आलोकित करता है और स्वयं निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार सब देहों में आत्मा एक है, यह समस्त शरीरों को आलोकित करता हुआ भी। स्वयं शुद्ध पवित्र रहता है, लिप्त नहीं होता।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ।।३४ ।।
शब्दार्थ : क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः-क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के मध्य, एवम् - इस प्रकार, अन्तरम् -भेद को, ज्ञानचक्षुषा-ज्ञान चक्षु से, भूतप्रकृतिमोक्षम् - प्राणियों का प्रकृति से मोक्ष, च-और, ये-जो, विदुः - जानते हैं, यान्ति-प्राप्त होते हैं, ते-वे, परम् -परमात्मा को ।
अनुवाद : जो लोग ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अन्तर और प्रकृति से जीवात्मा की मुक्ति को जान लेते हैं वे सर्वोच्च परमात्मा को प्राप्त होते हैं।
व्याख्या : शास्त्रों के अध्ययन और गुरु के उपदेश तथा ध्यानाभ्यास से खुले ज्ञान चक्षु के द्वारा जो यह जान लेते हैं कि क्षेत्र जड़ है, कर्ता है, परिणामी (परिवर्तनशील) है और प्रमेय (परिमित) है और क्षेत्रज्ञ (आत्मा) शुद्ध चेतन स्वरूप है, अकर्ता है, अव्यय है, अप्रमेय है तथा प्राणी का (अस्तित्व का) उपादान कारण अव्यक्त, अविद्या, प्रकृति का असत् भाव है और इन सब का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे परम तत्त्व परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आत्म साक्षात्कार से वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, माया जाल और अविद्या के चंगुल से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं।
सांख्य दर्शन के अनुसार बन्धन और मोक्ष आत्मा में नहीं होते क्योंकि यह सर्वदा विरक्त है, अकर्ता है, अभोक्ता है और अवयव रहित अखण्ड है। प्रकृति के साथ संयोगवश अध्यारोपण के द्वारा यह आत्मा कर्तृत्वभाव को प्राप्त होता है। आत्म-ज्ञान से जब अविद्या का विनाश हो जाता है तब आत्मा से संयुक्त प्रकृति मुक्त हो जाती है। तब आत्मा के समक्ष उसका नृत्य अथवा क्रीड़ा समाप्त हो जाते हैं। पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति ने जो कार्य करना था वह अब निःशेष हुआ। इसीलिए सांख्यवादी घोषणा करते हैं कि बन्ध और मोक्ष प्रकृति की ही अवस्थायें हैं। कुछ इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि | प्रकृति के चंगुल से और विकारों से आत्मा को मुक्त किया जाता है।
(इस अध्याय को प्रकृति-पुरुष-विभाग-योग भी कहा जाता है)।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३ ।।
।। इति क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ चतुर्दशोऽध्यायः
गुणत्रयविभागयोगः
श्री भगवानुवाच
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।।१ ।।
शब्दार्थ : परम् -परम, भूयः-पुनः, प्रवक्ष्यामि कहूँगा, ज्ञानानाम् - सब ज्ञानों में, ज्ञानम् ज्ञान, उत्तमम् - उत्तम, यत्-जो, ज्ञात्वा-जान कर, मुनयः मुनि जन, सर्वे सब, पराम् -परम, सिद्धिम् -पूर्णत्व को, इतः- यहाँ से (इहलोक से), गताः - प्राप्त हो गये।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : सब प्रकार के ज्ञान में उत्तम ज्ञान को अब मैं पुनः (तुमसे) कहूँगा जिसे जान कर समस्त मुनि जन इस जीवन के उपरान्त पूर्णत्व को प्राप्त हुए हैं।
व्याख्या : क्षेत्र का आगे का वर्णन इस अध्याय में दिया गया है।
अध्याय XIII के श्लोक २१ में यह उपदेश किया गया है कि शुभाशुभ योनियों में संसार में जन्म लेने का मूल कारण आसक्ति है। इस अध्याय में भगवान् कतिपय प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वे प्रश्न इस प्रकार हैं-प्रकृति के गुण क्या है? वे मनुष्य को बन्धन में कैसे डालते हैं? इन गुणों की विशेषतायें क्या हैं वह किस प्रकार व्यापार (चेष्टा) करते हैं? उन से मोक्ष कैसे सम्भव है? जीवन्मुक्त की विशेषतायें क्या हैं?
अध्याय XIII के श्लोक ७ से १० में सब ज्ञानों का कहीं वर्णन नहीं है किन्तु यह यज्ञादि से सम्बद्ध ज्ञान का उपदेश है। यज्ञादि का ज्ञान मोक्षप्रद नहीं है। किन्तु इस अध्याय में जो ज्ञान दिया जायेगा वह निश्चित रूप से मोक्ष प्रदान कराने वाला है। भगवान् इस ज्ञान को 'परम' और 'उत्तम' शब्दों से अभिहित करते हैं। अर्जुन को तथा अन्य साधकगण को उत्प्रेरित करने के भाव से ऐसा भगवान् ने कहा ।
इस परम ज्ञान की प्राप्ति पर मुनिजनों ने (जिन्होंने मनन किया) इस शरीर को त्यागने के उपरान्त मोक्ष प्राप्त किया।
इतः इस जीवन के उपरान्त । देह बन्धन से मुक्त होने पर।
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।।२ ।।
शब्दार्थ : इदम् - इस, ज्ञानम्-ज्ञान, उपाश्रित्य-शरण में आकर, मम-मेरे, साधर्म्यम् - एकत्व, आगताः- आ गये (प्राप्त किया), सर्गे-सृष्टि के समय, अपि-भी, न -नहीं, उपजायन्ते-उत्पन्न नहीं होते, प्रलये-प्रलय काल में, न-नहीं, व्यथन्ति-व्याकुल होते हैं, च-और।
अनुवाद : इस ज्ञान में आश्रित मनुष्यों ने मेरे साथ एकत्व प्राप्त कर लिया है। न तो सृष्टि के उद्भव काल में वे जन्म लेते हैं और न ही प्रलय काल में व्याकुल होते हैं।
व्याख्या : इस ज्ञान का आश्रय लेकर मुनिजन मेरी ही प्रकृति को अर्थात् मेरे सारूप्य-धर्म को प्राप्त होते हैं। वे मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने मेरे साथ एकत्व स्थापित कर लिया है। वे 'अहम्' और 'त्वम्' का विचार त्याग कर मुझ में निवास करते हैं तथा संसार चक्र को पार कर जाते हैं। उनके लिए सृष्टि और प्रलय का कोई भाव नहीं रह जाता। मुझे प्राप्त कर के वे अमरत्व, नित्यता और पूर्णता को प्राप्त होते हैं। समुचित साधनों द्वारा आत्म ज्ञानी ज्ञान प्राप्त कर के मुझमें एकीभाव हो कर न तो सृष्टि के आदि में जन्म लेते हैं न प्रलय में विनष्ट होते हैं। इस श्लोक में भगवान् ने आत्म-ज्ञान की प्रशंसा की है।
मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्नार्थं दधाम्यहम् ।
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।।३ ।।
शब्दार्थ : मम-मेरी, योनिः-योनि (गर्भ), महत् -महान, ब्रह्म-ब्रह्म, तस्मिन् - उसमें, गर्भम् बीज, दधामि-धारण करता हूँ, अहंम -मैं , संभवः- जन्म, सर्वभूतानाम् -सब प्राणियों का, ततः- वहाँ से, भवति होता है, भारत-हे भरतवंशी अर्जुन ।
अनुवाद : महत् ब्रह्म, हे अर्जुन, मेरी योनि है, उसमें मैं बीज धारण करता हूँ जो समस्त प्राणी समुदाय को जन्म देने वाला है।
व्याख्या : मेरा गर्भ महत् प्रकृति है। उस (परमात्मा) की प्रकृति से विश्व का उद्भव होता है 'प्रकृति' को महत् ब्रह्म कहते हैं क्योंकि वह वैश्विक मन और पाँच सूक्ष्म भूतों का आश्रय स्थल है। उसी अप्रकट से, सृष्टि प्रकट होती है इसीलिए उसे महत् ब्रह्म कहते हैं।
इसी महत् प्रकृति से समस्त विकार उत्पन्न होते हैं। अतः इसे मूलप्रकृति कहते हैं। अप्रकट होने से अव्यक्त कहते हैं। वेदान्ती उसे माया कहते हैं। सांख्यवादी उसे प्रकृति कहते हैं।
यह प्रकृति महत् कही जाती है क्योंकि यह अपने सब कार्यों (प्रभावों) से महती है। तीन गुणों से युक्त यह प्रकृति सब भूतों की उपादान कारण है। अपने समस्त विकारों का स्रोत और अपनी शक्ति के द्वारा उन विकारों को स्थिति प्रदान करने के कारण इसे ब्रह्म कहते हैं।
मैं इस महद्ब्रह्म में जीवन का बीज डालता हूँ तब सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। महद्ब्रह्म (प्रकृति) में मैं हिरण्यगर्भ का बीज निक्षेप करता हूँ जो समस्त प्राणियों को और वस्तुओं को रूप प्रदान करता है। हिरण्यगर्भ अथवा ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता) का उद्भव प्राणियों को अस्तित्व प्रदान करता है। मूल प्रकृति मानो मिट्टी के समान है। वह स्वयं से रूप प्रकट करने में असमर्थ है। प्रकृति से ब्रह्मा का उद्भव होता है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से सृष्टि की उसी प्रकार रचना करते हैं जैसे एक कुम्हार मिट्टी का पात्र बनाता है। मैं अपरा और परा, दो शक्तियों से युक्त हूँ (VII.4.5.), क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ (आत्मा और प्रकृति) का मैं संयोग करता हूँ। व्यष्टि आत्मा अविद्या, काम और कर्म के सीमित प्रतिबन्धों से प्रभावित होती है। अविद्या के कारण जीवात्मा अपनी मूल दिव्य प्रकृति को भूल जाता है और काम तथा कर्म के जाल में फंस कर जन्म-मृत्यु के चक्र में भ्रमण करता है। जीवात्मा अपनी वास्तविक दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ होने के कारण अविद्या की ओर अभिमुख होता है। अविद्या और प्रकृति के विकारों से अभिभूत हो कर जीवात्मा अपनी पूर्व पवित्रता को भूल कर विभिन्न रूपों में भ्रमण करता रहता है (अर्थात् जन्म-मरण के चक्र में फंस कर पृथक् पृथक् योनियों के रूप धारण करता है)।
अव्यक्त प्रकृति अमित शक्तियों का अन्धकारपूर्ण गर्भ है। यह कोई द्रव्य नहीं है। ध्वनि और शक्ति अव्यक्त रूप में इसमें निहित हैं। महाप्रलयकाल में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इसी में विलीन होता है। इस (प्रकृति) के तीन गुणों के मध्य द्रव्य अथवा गुण का कोई सम्बन्ध नहीं है। त्रैत साम्यावस्था में (तीन गुणों की साम्यावस्था) गुण ही मूल प्रकृति हैं और मूल प्रकृति ही गुण है।
इस त्रिगुणात्मक जगत् की तुलना एक बटी हुई रस्सी से की गई है जिसके तीन वर्ण हैं—सात्त्विक-श्वेत वर्ण है, राजसिक-रक्त वर्ण है और तमस् श्याम वर्ण है। प्रकट (व्यक्त) जगत् में यह तीन गुण साम्यावस्था में नहीं होते।
जल और बीज का पृथ्वी के साथ संयोग होने पर बीज अंकुरित होता है जो वृक्ष का रूप धारण करता है। प्रकृति के गर्भ में बीज आठ प्रकार के तत्त्वों में विकसित होता है-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार । आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग का प्रथम फल (परिणाम) है महत्तत्त्व अथवा बुद्धि । बुद्धि से मन की उत्पत्ति होती है, मन से अहंकार और अहंकार से पाँच तत्त्व उत्पन्न होते हैं।
प्राणियों की चार प्रजातियाँ हैं-जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज। जरायु (गर्भ का बहिर्वेष्टन, झिल्ली) से उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य, गाय, हाथी, घोड़ा आदि। इस जाति में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ विद्यमान रहती हैं। अण्डज अण्डे से उत्पन्न होते हैं। इस प्रजाति में वायु तत्त्व और आकाश तत्त्व की प्रधानता रहती है। स्वेदज की जाति में जूँ आदि जीव आते हैं जो पसीने (स्वेद) से उत्पन्न होने वाले हैं। इस प्रजाति में अग्नि और जल तत्त्व प्रधान होते हैं। बीज से उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि उद्भिज की संज्ञा से अभिहित हैं। इसमें पृथ्वी और जल तत्त्व की प्रधानता रहती है। (निरूपण - VII.6; IX. 17; XV.7)
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।।४ ।।
शब्दार्थ : सर्वयोनिषु सब योनियों में, कौन्तेय-हे कुन्ती पुत्र, मूर्तयः- भूर्ताकार रूप, सम्भवन्ति-होते हैं, या:-जो, तासाम्-उनमें, ब्रह्म-ब्रह्म, महत्-महान्, योनिः- योनि, अहम् -मैं, बीजप्रदः- बीज प्रदान करने वाला, पिता-पिता ।
अनुवाद : हे अर्जुन, किसी भी योनि में जो भी शरीराकार उत्पन्न होते हैं, महत् ब्रह्म (माया) रूप तो गर्भ धारण करने वाली योनि है और मैं (ईश्वर) बीज प्रदान करने वाला (गर्भाधान करने वाला) पिता हूँ।
व्याख्या : अहं पिता-महत् प्रकृति माता है। समस्त प्रकट रूप विश्व शिशु है जो प्रकृति ने मेरे संयोग से उत्पन्न किया है। इसीलिए मुझे विश्व का पिता कहा जाता है।
योनियाँ-देव, पितर, मनुष्य, घास चरने वाले पशु, वन्य पशु (मृग), पक्षी आदि।
मूर्तयः रूप-पृथक् पृथक् अङ्ग, अवयवों सहित शरीर ।
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ।।५ ।।
शब्दार्थ : सत्त्वम् - पवित्रता, रजः-काम, तमः- अविद्या, जड़ता, इति-इस प्रकार, गुणाः- गुण, प्रकृतिसंभवाः-प्रकृति से उत्पन्न, निबध्नन्ति-बाँधते हैं, महाबाहो - हे महाबाहो, अर्जुन, देहे—शरीर में, देहिनम् - शरीरी (आत्मा) को, अव्ययम् अनश्वर ।
अनुवाद : हे अर्जुन, (भगवान् की माया) प्रकृति से उत्पन्न सतत्त्व, रज और तम ये गुण इस शरीर में अविनाशी देही (आत्मा) को मानो बांध लेते हैं।
व्याख्या : सत्त्व गुण उत्तम है। रजस् इसके पश्चात् है और तमस् निम्न और निकृष्ट श्रेणी में गिना जाता है। तीन गुण तीन प्रकार की मानसिकता को उपलक्षित करते हैं। वे जीवात्मा में आसक्ति को जन्म दे कर उन्हें भ्रमित करते हैं और संसार के बन्धन में डालते हैं। शैशव, यौवन और वृद्धावस्था जैसे एक ही शरीर में अभिव्यक्त होते हैं उसी प्रकार तीन गुण मन की स्वाभाविक अवस्था में अन्तर्निहित हैं। प्रकृति के गुणों और शरीर के साथ जब आत्मा एकरूपता समझने लगता है तो बन्धन में आता है। परमात्मा से एकरूपता करने तक की अवधि पर्यन्त यह जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख और हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वों में अनुभव लेता रहता है। गुण शब्द प्रायः किसी द्रव्य के आश्रित 'गुण' के अर्थ में लिया जाता है जो किसी उपाधि, गुण अथवा वस्तु विशेष की ओर संकेत नहीं करता जैसे किसी वस्त्र का नील वर्ण। यहाँ नील वर्ण वस्त्र की विशेषता अथवा गुण को इङ्गित करता है किन्तु प्रकृति के गुण वस्तुतः प्रकृति के मूल घटक हैं और समस्त वस्तु विषयों का आश्रय हैं। इसलिए इन गुणों को किसी 'द्रव्य के आश्रित' रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए।
यदि तुम मुक्त हो कर पूर्णता की कामना करते हो और अविनाशी बनना चाहते हो तो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठो । त्रिगुणातीत बन जाओ।
पात्र में जल यदि हिल रहा है तो उसमें प्रतिबिम्बित सूर्य भी प्रतिबिम्ब अध्यास के कारण हिलता हुआ ही दृष्टिगत होगा। इसी प्रकार अध्यास द्वारा शुद्ध स्वरूप आत्मा प्रकृति के गुणों के बन्धन में आया हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा नित्य मुक्त, बन्धन रहित निरञ्जन और गुणातीत है।
अविद्या रूप ये गुण सदा क्षेत्रज्ञ पर निर्भर रहते हैं। वे मानो क्षेत्रज्ञ को दृढ़ बन्धन में बांध लेते हैं। उसी को अपना आश्रय बना कर वे कार्य करते हैं।
गुणों का ज्ञान और उनके क्रिया कलाप (व्यापार) का ज्ञान अत्यावश्यक है। मुक्त होने का साधन केवल इन्हीं गुणों का पूर्ण ज्ञान ही है।
महाबाहो -जानु तक लम्बी और अतिशय सामर्थ्य से युक्त बाहु वाला पुरुष महाबाहु है। यह एक शुभ लक्षण है। योगियों और ऋषि-मुनियों की ऐसी लम्बी सुन्दर भुजायें होती हैं।
तीन गुण सब मनुष्यों में विद्यमान हैं। प्रकृति के इन तीन गुणों के कार्य से कोई भी मुक्त नहीं है। वे सतत नहीं हैं। कभी सत्त्व की प्रधानता (मनुष्य में) है तो कभी रजस् की और अन्य काल में तमस् की प्रधानता हो जाती है।
सत्व आलोक (प्रकाश) का प्रतीक है। इसमें समन्वय और अच्छाई अथवा पवित्रता विशेष हैं। रजस् गतिविधि (क्रियाशीलता) का प्रतीक है तो तमस् जड़ता और निष्क्रियता दर्शाता है।
इन तीन गुणों के तत्त्वाधान में गोचर पदार्थों का विश्लेषण करो। उनकी विशेषताओं को जानो । इन गुणों के साक्षी द्रष्टा बन कर रहो । स्वयं को उनके साथ एकरूप मत करो। अपने को उनसे पृथक् करो। शाश्वत आनन्द, शान्ति और अमरत्व की प्राप्ति करोगे । (निरूपण –XIII.22)
तन्त्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ।।६ ।।
शब्दार्थ : तत्र-इनमें, सत्त्वम् -सत्त्वगुण (पवित्रता), निर्मलत्वात् - निर्मल होने के कारण, प्रकाशकम् -प्रकाश देने वाला, अनामयम् स्वास्थ्य देने बाला, सुखसङ्गेन सुख की आसक्ति से, बध्नाति-बांधता है, ज्ञानसङ्गेन-ज्ञान की आसक्ति से, च-और, अनघ हे निष्पाप (अर्जुन) ।
अनुवाद : हे निष्पाप अर्जुन, इनमें सत्त्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशशील और स्वास्थ्यकर (सुखद) है किन्तु सुख और ज्ञान के सङ्ग से बांधने वाला है।
व्याख्या : सत्त्व स्फटिक की भाँति निर्मल है। यह सुख और ज्ञान का मानो जाल बिछाने वाला है। यह स्वर्ण श्रृंखला है। सात्त्विक मनुष्य स्वयं को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझ कर आनन्दमग्न होता है। अपने ज्ञान से वह फूला नहीं समाता । अपने सुखों और सुखद अनुभवों का विचार कर के उसका हृदय दर्प से फूल उठता है। वह सोचता है-"मैं सुखी हूँ। मैं ज्ञानी हूँ।" इस प्रकार अहंकारवश वह बन्धन में आ जाता है। वस्तुतः यह गुण क्षेत्र अर्थात् अन्तःकरण का ही धर्म है किन्तु सत्त्व के बल से, अध्यास द्वारा इसे आत्मा में आरोपित किया जाता है।
ज्ञान मार्ग में रजस् और तमस् अंधकूप के समान हैं।
सुखासक्ति एक भ्रान्ति है। अविद्या है। किसी विषय का धर्म विषयी का नहीं हो सकता। इच्छा से लेकर धृति (XIII.6) पर्यन्त सब धर्म (विषय रूप) क्षेत्र के हैं। अविद्या से अविवेक जन्म लेता है। इसी कारण जीवन नित्य-अनित्य और विषयी विषय के भेद का ज्ञान नहीं कर पाता।
ज्ञान, अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) की विशेषता है, आत्मा का नहीं। यदि यह आत्मा का धर्म होता तो इसमें आसक्ति और बन्धन के भाव का अभाव होता । सत्त्व ज्ञान के द्वारा आत्मा को बांधता है।
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ।।७ ।।
शब्दार्थ : रजः रजस्, रागात्मकम् -राग स्वरूप, विद्धि-जानो, तृष्णासङ्गसमुद्भवम् - इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न, तत्-वह, निबध्नाति-बांधता है, कौन्तेय-हे कुन्ती पुत्र, कर्मसङ्गेन-कर्म में आसक्ति के द्वारा, देहिनम् -देही (आत्मा) को ।
अनुवाद : हे अर्जुन, रजस् को रागात्मक स्वभाव वाला जानो जो तृष्णा और आसक्ति का स्रोत है। यह देही को कर्मासक्ति द्वारा बांधता है।
व्याख्या : रजोगुण गतिशीलता और आकांक्षा का प्रतीक है। राजसिक मनुष्य इच्छा और तृष्णा से पूर्ण होता है। तृष्णायें उसे कर्म करने के लिए बाध्य करती हैं। उन तृष्णाओं की पूर्ति में सहायक लोगों में वह मनुष्य आसक्त हो जाता है और उनसे घृणा करने लगता है जो तृष्णापूर्ति में बाधक बनते हैं। वह कर्म में आसक्त हो जाता है। वह व्यवसाय में प्रवृत्त होता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञादि, अनुष्ठान और दान कर्म करता है। इन्द्रिय-सुखों के पीछे वह भागता रहता है किन्तु उसकी इच्छायें, निरन्तर तेल द्वारा भड़कती अग्नि की भाँति कभी शान्त अथवा पूर्ण नहीं होर्ती । आत्मा कर्ता नहीं है, साक्षी द्रष्टा है किन्तु रजस् मनुष्य में यह भाव उत्पन्न करता है- "मैं कर्त्ता हूँ।" रजस् कामनाओं को सजीव रखते हुए मन को प्रसन्नता प्रदान करता है।
राजसिक मनुष्य कभी सन्तुष्ट नहीं होता। वह सदा लोभी और व्याकुल बना रहता है। जितना अधिक वह प्राप्त करता है उतना ही और अधिक वह लोभी-लालची बनता है। उसकी कामनायें गुणित होती हैं (बढ़ती हैं)। उसे कोई सन्तुष्ट नहीं कर सकता। करोड़पति, अरबपति बनना चाहता है। अग्नि में घृत डालते जायें तो और अधिक उग्रता से बढ़ती है। राजसिक मनुष्य की
विवेक शक्ति और बुद्धि नष्ट होने लगते हैं। उसकी मेधा बुद्धि दर्प के अन्धकार से आवृत होने लगती है। वह धन-वैभव के नशे (मद) में चूर रहता है। उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। बुद्धि विपर्यय (भ्रंश) के कारण वह दुःख में सुख का, शोक में हर्ष का और कष्ट में उत्सव का अध्यास करके आनन्दित होता है। उसका लक्ष्य है स्त्री और धन (कंचन और कामिनी)। उसका आराध्य देव कुबेर अथवा धन की देवी लक्ष्मी है।
नाम, आराम और यश के पीछे भागते हुए अनेक प्रकार की क्रियाओं में वह संलग्न हो जाता है।
नारी कटाक्ष, विद्युत्वेग और मीन की गति, द्रुतगति से सम्बद्ध हैं, किन्तु रजस् की गति इनसे भी अधिक तीव्र है। वह सोचता है- “मेरी संपन्नता नष्ट होने पर मेरा क्या होगा ?" इस प्रकार स्वयं को अनावश्यक रूप से चिन्ता ग्रस्त कर लेता है और विभिन्न क्रिया कलापों में संलग्न हो जाता है।
प्राप्त में आसक्ति और अप्राप्त की प्राप्ति की पिपासा उसमें बनी रहती है। वह प्राप्त वस्तुओं की सुरक्षा का प्रयत्न करता है। यही सङ्ग है। “मैं यह करूँगा तो यह फल मिलेगा। यह अनुष्ठान करूँगा तो स्वर्गप्राप्ति होगी।" इस प्रकार कर्म और कर्मफल में आसक्ति ही कर्म सङ्ग है।
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ।।८ ।।
शब्दार्थ : तमः जड़ता, तु-परन्तु, अज्ञानजम् - अज्ञान से उत्पन्न, विद्धि -जानो, मोहनम् - मोहित (भ्रमित) करने वाला, सर्वदेहिनाम् -समस्त प्राणियों का, प्रमादालस्यनिद्राभिः -प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा, तत्-वह, निबध्नाति-बन्धन में डालता है, भारत- हे भरत वंशी (अर्जुन) ।
अनुवाद : हे अर्जुन, समस्त देहधारी मनुष्यों को भ्रमित करने वाले तमस् को तुम अविद्या से उत्पन्न जानो । यह (तमोगुण), प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवों को बांधता है।
व्याख्या : तमस् - वह बन्धन में डालने वाली शक्ति है जिसमें आलस्य, तन्द्रा (कार्यविमुखता) और मूर्खतापूर्ण कार्य करवाने की प्रवृत्ति निहित है। तमस् से मोह और अविवेक उत्पन्न होते हैं। शरीर पर आत्मा का अध्यास करने वाले को यह बन्धन में डालता है। तामसिक मनुष्य शरीर की अनिवार्यताओं के दबाव में कार्य करता है। उसमें निर्णयात्मक बुद्धि का अभाव होता है। शरीर के अभावों से दुःखी हो कर जीवित रहने के लिए वह कार्य करता है। उसके कर्म तर्क विहीन होते हैं। वे तो अशिक्षित बोध के धरातल पर विद्यमान रहते हैं। उसकी इन्द्रियाँ मूढ़ होती हैं। वह मोहित हो जाता है और मूर्ख भी बन जाता है। जम्हाई अधिक लेता है। अत्यधिक सोता है। सोने की अभिलाषा उसमें बनी रहती है। कब, कहाँ, कैसे कार्य करना चाहिए; इसका उसे ज्ञान नहीं होता। किससे किस प्रकार बात करनी है, यह सदाचार भी उसमें नहीं होता। गलत रास्ते पर चलने में वह हर्ष का अनुभव करता है। कैसे व्यवहार करना है, दूसरों को कैसे सम्बोधन करना है, वह नहीं जानता। विचार शून्य और अज्ञानी है वह। वह स्मृतिहास का शिकार हो कर सब कुछ भूल जाता है। वह प्रमादिन् (असावधान) और तंद्रिल बन जाता है। निर्जीव वस्तु की अपेक्षा बस थोड़ा अधिक उसे माना जा सकता है।
प्रमादी मनुष्य नित्यानित्यवस्तुविवेक नहीं कर सकता। प्रमाद तो प्रकाश का, जो सत्त्व का कार्य है, शत्रु है। आलसी मनुष्य संघर्ष नहीं कर सकता । रजस् के प्रभाव-प्रवृत्ति का भी यह शत्रु है। निद्रा लयवृत्ति है (अज्ञान में लीन होने की अवस्था है) जो तमस् पर आधारित है। सत्त्व और रजस् के किये कार्यों का यह शत्रु है।
सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ।।९ ।।
शब्दार्थ : सत्त्वम् सत्त्व, सुखे-सुख में, सञ्जयति-नियुक्त करता है, रजः रजस्, कर्मणि-कर्म में, भारत- हे भरतवंशी, ज्ञानम्-ज्ञान को, आवृत्य ढक कर, तु-निस्सन्देह, तमः-तम, प्रमादे-प्रमाद में, संजयति- लगाता है, उत-किन्तु ।
अनुवाद : हे अर्जुन, सत्त्व गुण सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को आवृत कर के प्रमाद में नियुक्त करता है।
व्याख्या : सूर्य को जिस प्रकार श्याम मेघ ढक लेते हैं उसी प्रकार आत्म-ज्ञान रूपी प्रकाश को तमस् आच्छादित कर लेता है। कर्तव्य कर्म के प्रति विमुखता, कर्तव्य को भूल जाना, अविद्या और असावधानी के प्रति आसक्ति का सृजन तमोगुण के कारण होता है।
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ।।१० ।।
शब्दार्थ : रजः रजस्, तमः-तमस् (जड़ता), च-और, अभिभूय- अभिभूत कर के (दबा कर), सत्त्वम् -सत्त्व, भवति-होता है, भारत-है भारत, रजः रजस्, सत्त्वम् सत्त्व, तमः-तमस्, च-और, एव-ही, तमः-तमस्, सत्त्वम् - पवित्रता, रजः- क्रियाशीलता, तथा और।
अनुवाद : हे अर्जुन, रजस् और तमस् को दबा कर सत्त्व का उदय होता है। सत्त्व और तमस् के दबने से रजस् उदित होता है और सत्त्व और रजस् के अभिभूत होने पर तमस् अपना कार्य प्रारम्भ करता है।
व्याख्या : शरद् और ग्रीष्मर्तु के समाप्त होने पर जैसे शीत का प्रकोप होता है, मनुष्य जब न तो जाग्रत हो और न ही स्वप्नावस्था में हो तो जैसे उस पर सुषुप्ति का आधिपत्य होता है अर्थात् उस समय वह निद्राधीन होता है वैसे ही रजस् और तमस् के दब जाने पर सत्त्व का प्रभुत्व होता है जो लोगों को सुखद अनुभूति प्रदान करता है। सत्त्व के विकास की साधना अध्याय XVII और XVIII में वर्णित है।
समय-समय पर प्रत्येक गुण अपना कार्य करता है। एक ही समय में सारे गुण समन्वित रूप से कार्य नहीं कर सकते। एक गुण जब अन्य दो गुणों को अभिभूत कर के प्रभुता को प्राप्त होता है तो वह अपना प्रभाव दर्शाता है। सत्त्व से ज्ञान और सुख प्राप्त होता है। रजस् क्रिया को प्रेरित करता है। तमस् ज्ञान को आच्छादित कर के जड़ता, तन्द्रा, आलस्य, निद्रा और अविद्या को जन्म देता है। सत्त्व के आरोहण काल में मनुष्य विवेकी बनता है। उत्कृष्ट विचार उसके मन में हिलोरें लेने लगते हैं। उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है। मन इन्द्रिय-विषयों से निवृत्त हो कर अन्तर्मुख होने लगता है।
कौन सा गुण किस काल विशेष में प्रधान है अथवा उदित हो रहा है, यह कैसे जाना जाये। इसके लक्षण अथवा विशेषतायें क्या हैं? उत्तर आगामी श्लोक में निहित हैं।
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।।११ ।।
शब्दार्थ : सर्वद्वारेषु -सब द्वारों में (इन्द्रियों के द्वार), देहे -शरीर में, अस्मिन् -इस, प्रकाशः ज्ञान-प्रकाश, उपजायते-प्रदीप्त होता है, ज्ञानम् ज्ञान, यदा-जब, तदा-तब, विद्यात्-जान लो, विवृद्धम्-बढ़ा हुआ, सत्त्वम् -सत्त्व, इति-इस प्रकार, उत-निश्चित रूप से ।
अनुवाद : इस शरीर के इन्द्रिय रूप प्रत्येक द्वार से जब ज्ञान-प्रकाश प्रदीप्त हो तो सत्त्व की प्रधानता (वृद्धि) समझनी चाहिए।
व्याख्या : किसी गुण विशेष का प्रादुर्भाव होने पर मनुष्य में कुछ पृथक् विशेषतायें प्रकट होती हैं। मालती (चमेली) जिस प्रकार अपनी सुगन्ध दूर-दूर तक बिखेरती है उसी प्रकार सत्त्व सब दिशाओं में विकीर्ण होता है। तमस् को रजसू में और रजस् को सत्त्व में परिणत करो और अब सत्त्व में दृढ़तापूर्वक बने रहो। तुम्हें संवर्धित प्रकाश, शुचिता, शान्ति और समन्वय प्राप्त होगा। सत्त्व तुम्हें आगे बढ़ायेगा। परम प्रकाश का ऊर्ध्वाकर्षण मिलेगा। सात्त्विक आहार, जप, ध्यान, शास्त्राध्ययन, एकान्तवास, सत्संगति, प्रभु का भजन-कीर्तन और प्राणायाम सत्त्व के संवर्धन में सहायक हैं।
अन्तर्परीक्षण करो। भीतर झांको । गुणों को अवधानपूर्वक निहारो। जागरूक बनो। द्वारपाल की भाँति रहो। मानसिक फैक्ट्री के द्वार से केवल सात्त्विक गुणों को ही भीतर जाने दो। रजस् को वश में करो। तमस् को नियंत्रित करो। सत्त्व की संवृद्धि होने पर मन में चिर स्थिर शान्ति का वास होगा, आन्तरिक समन्वय, पूर्ण सौम्यता और निश्चल धैर्य प्राप्त होगा। कल्पना शक्ति स्पष्ट होगी। विवेक पर अज्ञान के मेघ आच्छादित नहीं होंगे। सूक्ष्म ज्ञान (मर्मज्ञता) का आभास होगा। अन्तर्ज्ञान के द्वार खुलेंगे। इन्द्रियाँ बाह्य विषयों की ओर नहीं दौड़ेंगी।
इन्द्रियाँ विषय ज्ञान की वीथियाँ हैं। वह आत्म दर्शन के लिए तोरण द्वार (gateway) हैं। शरीर के चक्षु, कर्ण आदि समस्त द्वारों में जब ज्योति का आविर्भाव होता है अथवा अन्तःकरण में जब बुद्धि वृत्ति प्रकट होती है तब ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान के लक्षण से सत्त्व की प्रधानता (संवृद्धि) को समझा जा सकता है। प्रसन्नता, प्रफुल्लता सत्त्व का दूसरा लक्षण है। जिस प्रकार ज्ञान और प्रसन्न मुद्रा से साधक सत्त्व संवृद्धि का संज्ञान लेता है उसी प्रकार यह भी ज्ञान से जान लेता है कि रजस् और तमस् कम हो रहे हैं।
श्रवण न करने योग्य विषय का कर्ण परिहार करेंगे। नेत्र अदर्शनीय विषय का दर्शन नहीं करेंगे। वाणी न बोलने योग्य बात नहीं कहेगी। मन इन्द्रिय-विषयों से आकृष्ट नहीं होगा। जप, ध्यान और संयम के द्वारा शुचिता का विकास होगा। सत्त्व की वृद्धि से ज्ञान की भी वृद्धि होगी। आत्म-ज्ञान की प्राप्ति हेतु सत्त्व ही एक विश्वसनीय साधन है। यह ज्ञान की आधारशिला है।
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ।।१२ ।।
शब्दार्थ : लोभः लोभ, प्रवृत्तिः - क्रियाशीलता, आरम्भः- आरम्भ, कर्मणाम् कर्मों का, अशमः-व्याकुलता, स्पृहा-इच्छा, लालसा, रजसिरजस् में, एतानि-ये, जायन्ते-उत्पन्न होते हैं, विवृद्धे-बढ़ने पर, भरतर्षभ - हे भरत श्रेष्ठ (अर्जुन) ।
अनुवाद : हे अर्जुन, रजस् के बढ़ जाने पर, लोभ, क्रियाशीलता, कर्मों (कार्यों) का आरम्भ, अशान्ति और लालसा-ये चिह्न उत्पन्न होते हैं।
व्याख्या : लोभः- लोभ । परद्रव्य को प्राप्त करने की आकाङ्क्षा। पर्याप्त धन होने पर भी और अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा ।
प्रवृत्तिः-सामान्य भाव से सांसारिक क्रिया कलाप में लगना।
अशमः - अशान्ति । सुख और आसक्ति आदि में उद्विग्नता।
"मैं यह करूँगा फिर वह काम करूँगा। दूसरा काम समाप्त करके तीसरा प्रारम्भ करूँगा।" कर्म, इच्छा और तृष्णा का कहीं अन्त नहीं है। इसे अशमः कहा जाता है।
स्पृहा-प्रायः सभी इन्द्रिय-विषयों की इच्छा (पिपासा)। ये समस्त लक्षण राजसिक वृत्ति का संकेत देते हैं।
राजसिक अशान्ति और गतिविधि को कर्मयोग अथवा दिव्य क्रिया समझ कर अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि वे समाज की निष्काम सेवा कर रहे हैं। किन्तु विश्लेषण किया जाये तो कहीं न कहीं उनका स्वार्थ निहित होता है। बहुधा लोग क्षण भर के लिए भी शान्त नहीं बैठ सकते। वे सोचते हैं कि इतस्ततः घूमनाफिरना और कुछ न कुछ कार्य करते रहना ही जीवन की पूर्णता है। योगी अथवा संन्यासी जो मन को प्रशान्त कर के स्थिर बैठता है, शारीरिक रूप से कोई कार्य नहीं करता वह संसार का सर्वाधिक कर्मशील मनुष्य है। दूसरी ओर, इधर-उधर भागने वाला और हर समय व्यस्त रहने वाला व्यक्ति सर्वथा कुछ भी नहीं करता। तुम्हें यह लोकविरुद्ध अथवा असत्याभास लगता होगा। वस्तुतः इस कथन के सत्य को ग्रहण करना और समझना अत्यन्त कठिन है। सत्त्व प्रचंड गतिविधि है। अत्यन्त वेग से घूमने वाला चक्र स्थिरता का आभास देता है। ऐसे ही सत्त्व है। ऐसा ही सात्त्विक मनुष्य है।
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।।१३ ।।
शब्दार्थ : अप्रकाशः प्रकाश का अभाव, अविवेक, अप्रवृत्तिः- निष्क्रियता, च-और, प्रमादः -प्रमाद, असावधानी, मोहः- मोह, एव-ही, च-और, तमसि तमस् में, एतानि-ये, जायन्ते-उत्पन्न होते हैं, विवृद्धे-बढ़ जाने पर, कुरुनन्दन-हे कुरुनन्दन अर्जुन ।
अनुवाद : अन्धकार (अविवेक), निष्क्रियता, असावधानी, मोह, हे अर्जुन, ये लक्षण तमस् के बढ़ जाने पर परिलक्षित होते हैं।
व्याख्या : तमस् की वृद्धि होने पर अविवेक, निष्क्रियता (कुछ न करने की प्रवृत्ति), कर्तव्य-विमुखता और भ्रम आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं।
अप्रकाशः - अन्धकार अर्थात् विवेक का अभाव ।
अप्रवृत्तिः- जड़ता, कर्म का अत्यन्त अभाव ।
प्रमादः असावधानी और मोह-भ्रम ये सब अन्धकार (अविवेक) के कार्य (प्रभाव) हैं। ये लक्षण तमस् की प्रधानता को इङ्गित करते हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर अर्थात् किसी भी काल में आध्यात्मिक उन्नति और सफलता प्राप्ति हेतु तमस् एक विशाल प्रतिबन्धक है। किसी भी मूल्य पर इसे नष्ट करना अनिवार्य है। कभी-कभी लोग तमस् में सत्त्व (शान्ति) का अध्यास करते हैं। तामसिक मनुष्य को 'शान्त योगी' की उपाधि से अलंकृत करते हैं। “सब प्रारब्ध का खेल है। यह सब माया है। कोई संसार नहीं है। मैं कर्म में क्यों संलग्न होऊँ? कर्म मुझे बन्धनयुक्त करेगा। मैं ब्रह्म हूँ।" यह आध्यात्मिकता नहीं है प्रत्युत् तमस् की पराकाष्ठा है।
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ।।१४ ।।
शब्दार्थ : यदा-जब, सत्त्वे सत्त्व में, प्रवृद्धे वृद्धि होने पर, तु-निस्सन्देह, प्रलयम् -मृत्यु को, याति -प्राप्त होता है, देहभृत् - देहधारी मनुष्यात्मा, तदा तब, उत्तमविदाम् -सर्वोच्च (भगवान्) को जानने वालों के, लोकान् लोकों को, अमलान् -विशुद्ध, प्रतिपद्यते -प्राप्त होता है।
अनुवाद : सत्त्व की प्रवृद्धि काल में जब देहधारी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो तत्त्वविदों के विशुद्ध लोकों को प्राप्त होता है।
व्याख्या : लोकानमलान्-विशुद्ध लोक-ब्रह्म लोक आदि जहाँ रजस् और तमस् का सर्वथा अभाव होता है।
उत्तम सर्वोच्च-हिरण्यगर्भ आदि देवता ।
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ।।१५ ।।
शब्दार्थ : रजसिरजस् में, प्रलयम्-मृत्यु को, गत्वा-प्राप्त हो कर, कर्मसङ्गिषु कर्मों में आसक्त लोगों में, जायते-जन्म लेता है, तथा-और, प्रलीनः-मृत्यु काल में, तमसि-तमस् में, मूढयोनिषु मूढ़ योनियों में, जायते-जन्म लेता है।
अनुवाद : रजस् के वृद्धिकाल में मृत्यु हो तो मनुष्य कर्म में आसक्त पुरुषों में जन्म लेता है और तमस् की वृद्धिकाल में मृत्यूपरान्त मूढ़योनियों (निम्न योनियों) में जन्म लेता है।
रजसि प्रलयं गत्वा-रजस् के वृद्धिकाल में मरने पर उसका जन्म कर्मसङ्गियों में होता है और जब पूर्ण रूप से तमस् छाया हो और उस समय मृत्यु प्राप्त हो तो मूढ़ योनियाँ जैसे पशु, पक्षी, सिंह, कीट आदि में जन्म लेता है।
मूर्ख, विवेकशून्य निम्न मनुष्य जाति में भी उसका जन्म हो सकता है। सम्भव है वह पशु-पक्षी आदि की योनि को प्राप्त न हो-यह एक अन्य विचारधारा है।
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ।।१६ ।।
शब्दार्थ : कर्मणः-कर्म का, सुकृतस्य-शुभ कर्म का, आहुः-कहते हैं, सात्त्विकम् -सात्त्विक, निर्मलम् -शुद्ध, फलम् -फल (परिणाम), रजसः- रजस् का, तु-निश्चित रूप से, फलम् -फल, दु:खम् -दु:ख, अज्ञानम् अज्ञान, तमसः तमस का, फलम् -फल।
अनुवाद : शुभ कर्मों का फल सात्त्विक और निर्मल कहा गया है और राजसिक कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से (कर्म विकृति वश) दुःख है और तामसिक कर्मों का फल अज्ञान है।
व्याख्या : सुकृतः सात्त्विक कर्म। सात्त्विक कर्मों का फल ज्ञान और आनन्द की प्राप्ति है।
आहुः- (वे) कहते हैं अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं।
रजस् का अर्थ है राजसिक कर्म क्योंकि इस श्लोक में कर्म की व्याख्या हो रही है। राजसिक कर्मों का फल कटु होता है। रजस् दुःख, निराशा और असन्तोष देने वाला है। राजसिक कर्म लोभ की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। मूल तृष्णा को पूर्ण करते करते नव तृष्णायें अंकुरित हो उठती हैं और लोभ का द्वार खुलने लगता है।
तमस्-तामसिक कर्म, अधर्म कर्म । तमस् की प्रधानता में ज्ञान और दूरदर्शिता का अभाव रहता है।
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।।१७ ।।
शब्दार्थ : सत्त्वात् -सत्त्व से, संजायते-उत्पन्न होता है, ज्ञानम् - ज्ञान, रजसः रजस् से, लोभः- लोभ, एव-ही, च-और, प्रमादमोहौ-प्रमाद और मोह, तमसः-तमस् से, भवतः - होते हैं, अज्ञानम्-अज्ञान, एव-ही, च-और।
अनुवाद : सत्त्व से ज्ञान का उदय होता है, रजस् से लोभ और तमस् से प्रमाद, मोह और अज्ञान उदित होते हैं।
व्याख्या : सत्त्वात् सत्त्व से। सत्त्व के उत्कर्ष में ज्ञान जाग्रत होता है। जैसे सूर्य दिवस का प्रकाश लाता है उसी प्रकार सत्त्व बुद्धि को प्रकाशित करता है।
लोभ अग्नि की भाँति असन्तुष्ट रहता है। लोभ दुःख और पीड़ा का जनक है। इसकी उत्पत्ति रजस् से होती है। रजस् कभी पूर्ण न होने वाली तृष्णाओं को उत्पन्न करता है। राजसिक व्यक्ति दूसरों के भाव और रुचि के प्रति अन्धा सा हो जाता है। अपनी प्रगति और उत्कर्ष के लिए राजसिक व्यक्ति दूसरों को भी साधन बनाता है।
तामसिक व्यक्ति में दूरदर्शिता का अभाव, जड़ता और अज्ञान आदि लक्षण प्रधान होते हैं। भावी परिणामों के विषयों में तामसिक व्यक्ति सर्वथा विचारशून्य रहता है। वह पूर्ण रूप से शरीर के साथ एकरूप होता है और यदि कोई व्यक्ति उसे चोट पहुँचाये अथवा उसके विषय में कुछ बुरा कह दे तो वह लड़ने को आतुर रहता है। बदले के भाव में वह किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने को उद्यत रहता है। न तो उसका चित्त शान्त होता है और न ही उसमें सन्तुलन होता है।
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ।।१८ ।।
शब्दार्थ : ऊर्ध्वम् - उच्च स्थान को, गच्छन्ति-जाते हैं, सत्त्वस्थाः सत्त्व में स्थिर (मनुष्य), मध्ये-मध्य में, तिष्ठन्ति-रहते हैं, राजसाः- राजसिक, जघन्यगुणवृत्तिस्थाः जघन्य (निन्दनीय) गुणों में स्थित (मनुष्य), अधः - निम्न (योनियों में), गच्छन्ति-जाते हैं, तामसाः-तामसिक ।
अनुवाद : सत्त्व में स्थित पुरुष (देवादि) उच्च योनियों में जाते हैं। राजसिक मध्य में अर्थात् मनुष्य आदि योनियों को प्राप्त होते हैं और तामसिक मनुष्य जघन्य वृत्ति के कारण निम्न योनियों (पशु, पक्षी आदि) में उत्पन्न होते हैं।
व्याख्या : सत्त्वस्थ पुरुष इस शरीर को त्यागने के पश्चात् स्वर्ग के अधिपति बनते हैं। राजसिक मनुष्य पुनः इसी धरा पर जन्म लेते हैं। तामसिक व्यक्ति का पशु, मृग आदि निम्न योनियों में पतन होता है। मनुष्यों में निम्न वर्ग में भी उनका जन्म हो सकता है। मनुष्य जाति में निम्नतम वर्ग नृशंस, क्रूर मनुष्यों का है जो मनुष्य का शरीर धारण कर के भी पशुतुल्य हैं। उनके कर्म क्रूर होते हैं। अतः आवश्यक नहीं कि वे पशु जगत् में उत्पन्न हों।
मिथ्या ज्ञान अथवा भ्रान्ति पूर्ण ज्ञान के कारण मनुष्य प्रकृति के गुणों में आसक्त होता है और प्रकृति से एकरूप हो जाता है। उच्च अथवा निम्न योनियों में जन्म लेने का यही मुख्य कारण है। गुणों में अनुराग के कारण ही वह कभी दुःखी, कभी सुखी और कभी भ्रमित होने का अनुभव करता है।
गुणों की प्रकृति, उनके कार्य, वे (गुण) मनुष्य को संसार में बन्धक कैसे बनाते हैं, प्रत्येक गुण का कार्य (प्रभाव) जब उसकी प्रधानता होती है और पृथक् पृथक् गुण विशेष की संवृद्धि काल में विलय होने पर मनुष्य कौन-कौन से धाम को जाता है, इन सब का वर्णन पूर्व श्लोकों में हो चुका है। अब भगवान् आगामी श्लोक में यह उपदेश देते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति त्रिगुणातीत होने पर होती है।
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।।१९ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, अन्यम्-अन्य, गुणेभ्यः- गुणों से, कर्तारम् -कर्ता, यदा-जब, द्रष्टा देखने वाला, अनुपश्यति-देखता है, गुणेभ्यः- गुणों से, च-और, परम् - उच्चतर, वेत्ति-जानता है, मद्भावम् - मेरे भाव को, सः वह, अधिगच्छति-प्राप्त होता है।
अनुवाद : जब द्रष्टा गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता रूप में नहीं देखता और उन (गुणों) से ऊपर साक्षी परमात्मा को उनसे अतीत जान लेता है तब वह मेरे भाव को प्राप्त होता है।
व्याख्या : परमात्मा किसी भी प्रकार से गुणों में लिप्त नहीं होता। मुक्त 'संन्यासी घोषणा करता है- "मैं गुणों का साक्षी हूँ। न तो मैं कर्ता हूँ और न ही भोक्ता हूँ। समस्त कर्मों के पीछे प्रेरक शक्ति गुण ही हैं। मैं गुणों से परे हूँ। समस्त कर्मों के लिए गुण ही उत्तरदायी हैं। मैं इन गुणों से सर्वथा पृथक् हूँ। मैं शुद्धचैतन्य स्वरूप हूँ। गुण मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। मैं आकाश वत् हूँ।
गुण ही शरीर, इन्द्रिय एवम् अन्य विषयों रूपी विकारों को प्राप्त होते हैं, गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्त्ता नहीं-इस प्रकार के ज्ञान से जब आत्मा
देदीप्यमान होता है तब मनुष्य को यह ज्ञान भली प्रकार हो जाता है कि समस्त परिणामों (विकृतियों), अवस्थाओं और कर्मों में गुण ही कर्ता हैं और परमात्मा त्रिगुणातीत, गुणों का मौन साक्षी और उनकी प्रतिक्रियाओं का द्रष्टा है, तब वह मेरे साथ सारूप्य भाव को प्राप्त होता है। वह गुणातीत (गुणों से परे) हो जाता है।
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ।। २० ।।
शब्दार्थ : गुणान् गुणों को, एतान्-इन, अतीत्य उल्लंघन करके, त्रीन्-तीन, देही देहधारी, देहसमुद्भवान् - देह जिनसे उत्पन्न हुआ है, जन्ममृत्युजरादुःखैः जन्म, मृत्यु, जरा और दुःखों से, विमुक्तः मुक्त, अमृतम् - अमृतत्व, अश्नुते - प्राप्त करता है।
अनुवाद : देह की उत्पत्ति के बीज स्वरूप इन गुणों का अतिक्रमण-कर के देहधारी पुरुष जन्म, मृत्यु, क्षय और दुःख से मुक्त हो कर अमृतत्व की प्राप्ति करता है।
व्याख्या : एक नदी जैसे सागर में विलीन हो जाती है वैसे ही इस शरीर के बीज भूत गुणों का अपने जीवन काल में ही अतिक्रमण करने वाला पुरुष मुझ में लीन होता है। वह सदा शाश्वत शान्ति का आनन्द लेता है। मोक्ष प्राप्त करता है। मेरे भाव को प्राप्त होता है। भगवान् ने जब कहा कि मनुष्य गुणातीत हो कर अमरत्व को प्राप्त कर सकता है तो अर्जुन को और अधिक ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा हुई। अध्याय II के श्लोक ५४ में जैसे अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ की परिभाषा जानने के लिए भगवान् से प्रश्न किया था वैसे ही अब वह भगवान् कृष्ण से उस महापुरुष की विशेषतायें जानने का इच्छुक है जिसने तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लिया हो। वह कैसे चेष्टा करता है? उसका व्यवहार क्या है? वह तीन गुणों से अतीत किस विध हुआ?
अर्जुन उवाच
कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।
किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ।।२१ ।।
शब्दार्थ : कैः-किन किन, लिङ्गः लक्षणों से, त्रीन-तीन, गुणान् - गुण, एतान् -इन, अतीतः-अतीत, भवति-होता है, प्रभो हे भगवन्, किमाचारः-कैसा आचरण, कथम् -कैसे, च-और, एतान् -इन, त्रीन्-तीन, गुणान् गुणों को, अतिवर्तते - अतिक्रमण करता है।
अनुवाद : हे प्रभो, त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है? उसका आचरण कैसा होता है और वह इन तीन गुणों से अतीत कैसे पहुँचता है?
व्याख्या : अर्जुन ने कहा- "किन किन विशेषताओं से त्रिगुणातीत विद्वान् का संज्ञान होता है? उसका आचार-व्यवहार कैसा होता है और वह संसार से और गुणों से ऊपर कैसे उठता है? कृपया उपदेश करें।"
त्रिगुणातीत विद्वान् के यह लक्षण हैं। अन्य विद्वानों को भी इन गुणों (लक्षणों) का संवर्धन करना चाहिए।
एक राजा जिस प्रकार अपने सेवकों के दुःख-दर्द की निवृत्ति करता है उसी प्रकार भगवान् अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। तभी तो अर्जुन भगवान् कृष्ण को 'प्रभु' कह कर सम्बोधित कर रहे हैं। इस शब्द का प्रयोग कर के अर्जुन ने भगवान् को यह संकेत कर दिया है कि केवल वे ही उसकी पीड़ा का हरण करने में समर्थ हैं। (निरूपण - II.54)
श्री भगवानुवाच
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ।।२२ ।।
शब्दार्थ : प्रकाशम् - प्रकाश, च-और, प्रवृत्तिम् - प्रवृत्ति (क्रिया- शीलता), च-और, मोहम् -मोह, एव-ही, च-और, पाण्डव-हे अर्जुन, न-नहीं, द्वेष्टि-द्वेष करता है, संप्रवृत्तानि-उद्भूत, न-नहीं, निवृत्तानि-निवृत्त होने पर, काङ्क्षति-चाहता है (इच्छा करता है)।
अनुवाद : प्रकाश (सत्त्व), प्रवृत्ति (रजस्) और मोह (तमस्) की विद्यमानता में वह (त्रिगुणातीत) इनसे द्वेष नहीं करता और इनके अभाव में इनकी अभिलाषा नहीं करता।
व्याख्या : अर्जुन के प्रथम प्रश्न का यह उत्तर है। प्रकाश सतत्त्व का कार्य है, गतिविधि रजस् का और मोह तमस् का कार्य है। विषयभाव से उपलब्ध होने पर जीवन्मुक्त इनसे द्वेष नहीं करता। सत्त्व का प्रकाश होने पर वह अहंकार नहीं करता। वह यह नहीं सोचता - "मैं बहुत विद्वान हूँ।" शरीर जब कर्म में प्रवृत्त होता है अथवा लोकसंग्रह हेतु उसे दैवी आज्ञा से कर्म करने की प्रेरणा होती है तो वह किसी कर्म से द्वेष नहीं करता और कर्म की समाप्ति पर पश्चात्ताप नहीं करता । कर्म रत रहते हुए भी उनसे अनुशोक नहीं होता। कर्म तो उसके लिए बालक का खेल है। मोह की संवृद्धि पर वह भ्रान्त नहीं होता।
अयथार्थदर्शी अविद्यायुक्त मनुष्य ही ऐसा चिन्तन करेगा- "तमस् ने ये मझे घेर लिया है। मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मैं जड़ता, मूढ़ता, तन्द्रा, निद्रा, आलस्य के आधीन हो रहा हूँ। अब मैं रजस् के वश में हूँ। अब मुझे कार्य करना पड़ेगा। यह दुःखद है। मैं स्वप्रकृति से पतित हो गया हूँ। इससे मुझे बहुत दुःख हो रहा है। अब मैं सत्त्व के प्रभाव में हूँ। मैं ज्ञान और सुख में आसक्त हो रहा हूँ। अपने ज्ञान और विद्वत्ता का मुझे अभिमान हो गया है।"
मुक्त संन्यासी, जो त्रिगुणातीत है, उनकी विद्यमानता में उनसे द्वेष नहीं करता ।
एक सात्त्विक, राजसिक अथवा तामसिक मनुष्य प्रकाश, प्रवृत्ति अथवा मोह की कामना करता है जो अभिव्यक्ति के पश्चात् लुप्त हो गये। त्रिगुणातीत जीवन्मुक्त इन गुणों के लुप्त होने पर उनकी कामना नहीं करता। यह लक्षण मानसिक अवस्था का है। अन्य लोग इसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, न ही इसकी खोज कर सकते हैं। केवल मात्र स्वयं ही इस स्वयंवेद्य अवस्था की पहचान की जा सकती है। अन्तर्चक्षु अथवा दिव्य दृष्टि से जो विद्वान् इसका ईक्षण कर सकता है वह दूसरे मनुष्य के मन में जाग्रत हो रही इच्छा को भी स्पष्ट देख सकता है।
आगामी तीन श्लोकों में भगवान् अर्जुन के द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हैं-"त्रिगुणातीत पुरुष का आचरण कैसा होता है?"
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ।।२३ ।।
शब्दार्थ : उदासीनवत् - उदासीन की भाँति, आसीनः-स्थित, गुणैः गुणों के द्वारा, यः जो, न-नहीं, विचाल्यते-विचलित होते, गुणाःगुण, वर्तन्ते-बरत रहे हैं, इति-इस प्रकार, एव-ही, यः-जो, अवतिष्ठति-आत्मस्थ रहता है, न-नहीं, इङ्गते-विचलित होता है।
अनुवाद : उदासीन भाव से जो (विद्वान् संन्यासी) स्थित रहता है उसे गुण विचलित नहीं करते और जो यह जान लेता है गुण ही क्रियारत हैं (गुण ही गुणों में बरत रहे हैं) वह आत्मस्थित पुरुष विचलित नहीं होता।
व्याख्या : वह पक्षपात रहित हो कर अपने भाव में स्थित रहता है। वह राग-द्वेष से मुक्त होता है। गुण और शरीर रहें या न रहें वह इन सब से सर्वथा विरक्त रहता है। वह तो क्रिकेट मैच, फुटबाल मैच अथवा किसी नाटक का द्रष्टा रूप बन कर रहता है। वायु चलने से जैसे आकाश अप्रभावित रहता है उसी प्रकार गुणों के कार्य से वह सर्वथा उदासीन (निर्लिप्त) रहता है।
आत्म-साक्षात्कार के मार्ग से वह विचलित नहीं होता । दृढ़ संकल्प से वह मार्ग का अतिक्रमण करता है। वह सोचता है और अनुभव करता है-"गुण ही शरीर, मन, इन्द्रिय रूप में परिणत हुए हैं। वे एक-दूसरे पर अन्योन्य भाव से कार्यरत हैं, एक में एक बरत रहे हैं", ऐसा सोच कर वह उनसे विचलित नहीं होता। वह अपनी आत्मा में मेरु पर्वत के समान अडिग रहता है, दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है। (निरूपण - III.28.V.8-11)
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।।२४ ।।
शब्दार्थ : समदुःखसुखः सुख-दुःखख में समान, स्वस्थः स्वरूप में अवस्थित, समलोष्टाश्मकाञ्चनः-स्वर्ण, पाषाण खण्ड और मृत्तिका खण्ड को समान देखने वाला, तुल्यप्रियाप्रियः - प्रिय, अप्रिय में समान, धीरः- धीर, दृढ़, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः-निन्दा और स्तुति में सम ।
अनुवाद : सुख-दुःख में जो समान है, जो स्वस्थ है अर्थात् अपने स्वरूप में (आत्मा में) स्थित है, जिसके लिए स्वर्ण, पत्थर और मिट्टी समान हैं, जो प्रिय-अप्रिय में भेद नहीं रखता, जो धीर है (बुद्धिमान है) और जिसे अपनी निन्दा और स्तुति दोनों समान प्रतीत होते हैं।
व्याख्या : धरा पर गढ़े हुए स्तम्भ के लिए अहोरात्र का कोई अभिप्राय नहीं है। इसी प्रकार आत्मस्थित यति के लिए सुख और दुःख कोई प्रयोजन नहीं रखते। वह द्वन्द्रों से ऊपर है। उसकी दृष्टि में स्वर्ण अथवा गोमय (गोबर), मणि (हीरा) अथवा प्रस्तर (पत्थर) समान मूल्य के हैं। आदान-प्रदान के भाव से वह मुक्त है। प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु से वह सुखी और दुःखी नहीं हब से कूल-प्रतिकूल वस्तुओं में वह समभाव रहता है। निन्दा और स्तुति उसको प्रभावित नहीं करते। वह दृढ़ संकल्प रहता है। वह अपने सत्-चित्-आनन्द स्वरूप में स्थित रहता है। वह सदा शान्त और सौम्य रहता है। (निरूपण-V.18)
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।।२५ ।।
शब्दार्थ : मानापमानयोः मान और अपमान में, तुल्यः समान, तुल्यः समान, मित्रारिपक्षयोः-मित्र और शत्रु पक्ष में, सर्वारम्भपरित्यागी-दृष्ट अथवा अदृष्ट फल के लिए किये जाने वाले कर्मों (आरम्भ) का त्याग करने वाला, गुणातीतः गुणों से अतीत, सः-वह, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : जो मान-अपमान में, मित्र और शत्रु में समान है और समस्त आरम्भों का त्याग करने वाला है वह गुणातीत कहलाता है।
व्याख्या : मान-अपमान में वह अपना मन सन्तुलित रखता है। मित्र और शत्रु के लिए वह समरूप है। वह द्वन्द्वों से विचलित नहीं होता। वह गुणातीत हो चुका है। वह अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में अवस्थित रहता है। वह अपनी आत्मा में स्थित रहता है। वह प्रकृति के गुणों का अतिक्रमण कर चुका है। अब वह गुणों की क्रीड़ा से प्रभावित नहीं होता। सब विकारों (पर्यासों) में वह समदृष्टि रखता है। वह प्रशान्त साम्यावस्था बनाये रखता है।
दृष्ट अथवा अदृष्ट फल देने वाले समस्त कर्मों का वह त्याग कर देता है किन्तु शरीर के निर्वाह हेतु अनिवार्य कर्म करता है। श्लोक २३.२४.२५ में उदासीनता आदि गुण मोक्ष प्राप्ति में साधन हेतु हैं। वे तुम्हारे समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिनका अनुकरण करना चाहिए। साधक को उन गुणों का विकास करना चाहिए। किन्तु स्वरूप स्थिति में ही आत्म-ज्ञान सम्भव है। ये विशेषतायें उसके स्वभाव का अभिन्न अङ्ग बन कर यह दर्शाती हैं कि वह त्रिगुणातीत है।
अगले श्लोक में भगवान्, अर्जुन के तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं "तीन गुणों से ऊपर कैसे उठें?"
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।२६ ।।
शब्दार्थ : माम् -मुझे, च-और, यः- जो, अव्यभिचारेण - अविचलित भाव से, भक्तियोगेन-भक्ति योग से, सेवते-सेवा करता है, सः- वह, गुणान् गुणों को, समतीत्य-अतिक्रमण कर के, एतान् -इन, ब्रह्मभूयाय-ब्रह्म भाव के लिए, कल्पते-समर्थ होता है।
अनुवाद : अनन्य भक्तिभाव से जो मेरी सेवा करता है वह गुणातीत हो कर ब्रह्मभाव में स्थित होने के लिए समर्थ होता है।
व्याख्या : संन्यासी अथवा कर्मयोगी, सब के हृदयों में स्थित उस नारायण की अनन्य भक्तिभाव से सेवा करता है उसे आत्म साक्षात्कार होता है तत्पश्चात् वह गुणातीत हो कर आवागमन के चक्र से मुक्त होने, मोक्ष प्राप्ति करने अथवा ब्रह्म स्वरूप बनने के लिए शक्य हो जाता है।
भगवान् की अहेतुकी अनुकम्पा से वह आत्म-ज्ञान प्राप्त करता है। "प्रेम भाव से मेरी उपासना करने वाले सदा समन्वित उन भक्तों को मैं विवेक देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं।" "उनके प्रति अनुग्रह के भाव से, उनके अन्तःकरण में स्थित मैं अविद्या-जनित अन्धकार को प्रकाशमय ज्ञानदीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ।" (निरुपण - X .10.11)
अव्यभिचारिणी भक्ति-भक्त अनवरत रूप से भगवान् का ध्यान करता है। भक्त का भगवान् के प्रति अनन्य भक्ति भाव रहता है। भगवान् के अतिरिक्त अन्य कोई विचार उसके मन में नहीं उठता। भगवत् भाव से मन पूर्ण रहता है। तैलधारवत् उसके विचार भगवान् के प्रति निरन्तर चलते रहते हैं। सजातीय-वृत्ति-प्रवाह अर्थात् विचारों की अटूट श्रृंखला बनी रहती है। इन्द्रिय-विषयों के विचारों का पूर्ण अभाव रहता है। त्रिगुणातीत बनने के लिए भगवद् भाव का सतत प्रवाह विश्वस्त साधन है।
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याव्ययस्य च ।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ।।२७ ।।
शब्दार्थ : ब्रह्मणः ब्रह्म का, हि-निस्सन्देह, प्रतिष्ठा-आश्रय, अहम् -मैं, अमृतस्य अनश्वर का, अव्ययस्य-अविनाशी का, च-और, शाश्वतस्य-शाश्वत का, च-और, धर्मस्य-धर्म का, सुखस्य-आनन्द का, एकान्तिकस्य-सुख स्वरूप अर्थात् व्यभिचार रहित, आनन्दमय, च-और।
अनुवाद : क्योंकि मैं अव्यय और अमृत स्वरूप ब्रह्म का, धर्म का और परम आनन्द का आश्रय हूँ।
व्याख्या : अमर, अनश्वर आत्मा जो आत्म-ज्ञान के शाश्वत धर्म के द्वारा प्राप्य है और जो कभी क्षय न होने वाला आनन्द है, मुझ परमात्मा में प्रतिष्ठित है। मैं, अन्तरात्मा, परमात्मा की प्रतिष्ठा हूँ। आत्म-ज्ञान के पश्चात् दिव्य दृष्टि द्वारा साधक देखता है कि अन्तरात्मा ही परमात्मा है क्योंकि वही उसका निवास स्थान है।
अपनी शक्ति अथवा माया से भगवान् अपने भक्तों पर दया और कृपादृष्टि करते हैं। शक्ति और भगवान् अभिन्न हैं। अग्नि से जैसे उष्णता पृथक् नहीं है वैसे ही भगवान् की शक्ति उनसे पृथक् नहीं है। शक्ति भगवान् में प्रतिष्ठित है अतः पृथक् नहीं हो सकती।
एक और व्याख्या इस प्रकार है-ब्रह्म का अभिप्राय यहाँ सगुण ब्रह्म से है जो सोपाधिक है। मैं, परब्रह्म, तीन गुणों से अतीत हो कर उपाधिरहित निर्गुण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म (परमात्मा), सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा (आश्रय) हूँ जो नित्य है और अनश्वर है। ज्ञान-निष्ठा के परम धर्म का भी मैं आश्रय हूँ तथा अविचलित अनन्य भक्ति से उत्पन्न एकान्तिक आनन्द का भी मैं ही आश्रय हूँ।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ।।१४ ।।
।। इति गुणत्रयविभागयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ पञ्चदशोऽध्यायः
पुरुषोत्तमयोगः
श्री भगवानुवाच
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ।।१ ।।
शब्दार्थ : ऊर्ध्वमूलम् ऊपर की ओर मूल वाला, अधःशाखम् - नीचे शाखा वाला, अश्वत्थम् - अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष, प्राहुः-कहते हैं, अव्ययम् - अनश्वर, छन्दांसि वेद, यस्य-जिसके, पर्णानि-पत्ते, यः-जो, तम् - उसे, वेद- जानता है, सः वह, वेदवित्-वेदों का ज्ञाता है।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : वे (विद्वज्जन) अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष को ऊपर मूल और नीचे शाखा वाला कहते हैं जिसके पत्ते छन्द अर्थात् ऋचायें हैं। जो इसे जानता है वह वेदों को जानने वाला है (वेदज्ञ है)।
व्याख्या : पीपल के वृक्ष रूप में विश्व का वर्णन केवल रूपक भेद से अलंकारित है। यह पीपल शाश्वत कहा जाता है क्योंकि ज्ञान रूप खड्ग से ही इसको काटा जा सकता है।
कर्मफल के लिए सब मनुष्य भगवान् के आधीन हैं क्योंकि केवल वही कर्म और फल के सम्बन्ध को जानने वाला है। मनुष्यों को कर्मफल प्रदान करने वाला केवल वही है। ज्ञानी पुरुष भी अपने ज्ञान का फल पाने के लिए उसके आधीन है। अपनी कृपा दृष्टि से ईश्वर ही अज्ञान रूप आवरण को निवृत्त करता है। उसी की कृपा से वेदान्त-साधना की प्रेरणा होती है।
"भगवान् की कृपा से ही मन में एकत्व भाव उत्पन्न होता है जो सब प्रकार के भय से मुक्त करने वाला है।"-अवधूत गीता १.१
अनन्यमनस्क हो कर भगवान् की आराधना करने वाले साधक उनकी कृपा से त्रिगुणातीत हो जाते हैं। उनकी दया से आत्म-ज्ञान प्राप्त कर के वे जन्म-मृत्यु के बन्धन से परे हो जाते हैं। सम्यक् विवेक और यथार्थ ब्रह्म ज्ञान होने पर सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस उपदेश में भगवान् ब्रह्म की यथार्थ प्रकृति और आत्मा का उन तक पहुँचने का साधन बताते हैं। संसार की प्रकृति की उपमा भगवान् पीपल के वृक्ष से देते हैं, वे मनुष्य को विरक्ति का उपदेश देते हैं क्योंकि बिना वैराग्य के आत्म-ज्ञान सम्भव नहीं। संसार को वृक्ष की उपमा दी गई है क्योंकि वृक्ष की भाँति इसका भी उच्छेदन हो सकता है।
अन्य सभी वृक्षों की मूल नीचे की ओर होती है किन्तु इस संसार (माया) रूपी विशेष, अद्भुत, अलौकिक वृक्ष की मूल ऊपर की ओर है। अन्य सभी वृक्षों की अपेक्षा यह वृक्ष अनोखा है। सब पदार्थों का आश्रय ब्रह्म है। ब्रह्म शाश्वत है। ब्रह्म महान् है। ब्रह्म सर्वोच्च है। ब्रह्म परम पुरुष है। ब्रह्म सब वस्तुओं से श्रेष्ठ है। ब्रह्म सब पदार्थों का मूल स्रोत है। इसीलिए इसे एक अर्थात् अद्वितीय और ऊर्ध्व कहा है। सर्वोत्कृष्ट होने से ब्रह्म ही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण है।
पुराण में विवक्षित है- अव्यक्त वृक्ष ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। बुद्धि इसकी मूल है, इन्द्रियाँ इसके कोटर (शून्य गर्भ) हैं, महाभूत शाखा-प्रतिशाखा हैं, इन्द्रियों के विषय पत्ते हैं, अधर्म और धर्म सुन्दर पुष्प हैं, दुःख और सुख फल हैं। आत्म-ज्ञान रूपी श्रेष्ठ खड्ग द्वारा इस शक्तिशाली वृक्ष का छेदन कर के ब्रह्म का शाश्वत आनन्द प्राप्त कर के पुनः वहाँ से कोई नहीं लौटता।
इस वृक्ष का मूल ब्रह्म है। यह वृक्ष का ऊपरी भाग होने से ऊर्ध्व अभिहित है। यथार्थतः उस एक अखण्ड एकत्व में ऊर्ध्व, निम्न और मध्य रूप कोई भेद नहीं है।
अश्वत्थ नाम अ-श्वत्थ से बना है जिसका अभिप्राय है- "कल तक र रहने वाला"। अ का अर्थ 8 - 75f । श्व-आने वाला कल है और थ-स्थिरता के भाव में है। क्षणभङ्गुर, सदा परिवर्तनशील संसार-वृक्ष के लिए यह (अश्वत्थ) समुचित शब्द है।
कठोपनिषद् में भी इस अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन है (11.6.1)। गीता उपनिषदों का ही सार है।
संसार का अभिप्राय प्रायः इतना ही लिया जाता है कि मनुष्य की पत्नी हो, बच्चे हों, उनसे घिरा रहे और नित्य कर्तव्य-कर्म करता रहे। यह अत्यन्त संकुचित अर्थ है। संसार का अर्थ है- 'समस्त सृष्टि का प्रक्रिया-क्रम'। अथवा "वैश्विक अभिव्यक्ति" अथवा "नित्य परिवर्तित होने वाला संसारचक्र"। हिरण्यगर्भ, व्यष्टि आत्मायें, वैश्विक चेतना, अहंकार, मूल-महाभूत आदि इस संसार वृक्ष की शाखायें हैं। वे नीचे की ओर प्रवृत्त होती हैं। वे स्थूल से स्थूलतम अवस्थाओं को प्राप्त होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष की शाखायें नीचे की ओर हैं। अहंकार ही वह अंकुर है जो अधोगामी है और प्रकृति के तीन गुण रूपी तीन दिशाओं में प्रवृत्त होता है।
मन शाखा है। पंच महाभूत-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ शाखा-प्रतिशाखा हैं। इसके पश्चात् है ध्वनि जो कर्णों को मधुर संगीत श्रवण के लिए प्रेरित करती है। स्पर्श, त्वचा को कोमल स्पर्श का सुख लेने के लिए प्रेरित करता है। रूप चक्षु को सुन्दर लुभावना दृश्य देखने को प्रेरित करता है। रसना, जिह्वा को स्वादिष्ट पदार्थ के स्वाद के लिए प्रेरित करती है। गन्ध, नासिका को सुगन्धित विषय का सुख प्रदान करती है।
कर्मों के मूल से और फल की आशा से पुनर्जन्म रूपी नवीन शाखा उदित होती है। खनिज पदार्थ, वनस्पति संसार, पशु जगत् और मनुष्य जगत्-ये सब संसार वृक्ष की शाखायें हैं। मनुष्य शरीर की सहायता से शुभाशुभ कर्म करता है और परिणाम भोग हेतु पुनर्जन्म लेता है। मानव काया इस संसार वृक्ष का जल है।
शरीर स्वयं ही पीपल का वृक्ष है। मूल मेरुदण्ड में स्थित सुषुम्ना और स्नायु मण्डल (मस्तिष्क) है। विभिन्न शिरायें उपशाखा रूप में विभक्त हो कर, निम्नगामी होकर शरीर के विभिन्न अंगों में विभक्त हो जाती हैं।
अव्यय-शाश्वत । क्योंकि यह वृक्ष जन्मों की अनादि और अनन्त अटूट श्रृंखला पर आश्रित है। इस प्रकार से यह नित्य है। ब्रह्म-ज्ञान की खड्ग से इसे काटा जा सकता है। वृक्ष को जैसे पत्ते रक्षा प्रदान करते हैं वैसे ही वेद धर्म-अधर्म, उनके कारण और परिणाम को प्रकट करने वाले होने के कारण संसार रूपी वृक्ष की रक्षा करते हैं।
ऊपर वर्णित मूल सहित इस वृक्ष (विश्व वृक्ष) को जानने वाला, वेदों को अर्थात् वेदों के अर्थ को जानने वाला है। वह वेदों के उपदेश को जानने वाला है। मूल सहित इस संसार वृक्ष से अन्य जानने योग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है। इस प्रकार जानने वाला सर्वज्ञ है। साधकों को इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रेरणा देने के लिए भगवान् ने संसार वृक्ष के ज्ञान की स्तुति की है।
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
अधश्च मूलान्यनुसंततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।।२ ।।
शब्दार्थ : अधः नीचे, च-और, ऊध्वं-ऊपर, प्रसृताः-फैली हुई, तस्य-उसकी, शाखाः-शाखायें, गुणप्रवृद्धाः- गुणों से पोषित, विषयप्रवालाः- जड़ें, मूल, अधः नीचे, च-और, मूलानि-जड़ें, मूल, अनुसंततानि-विस्तृत, कर्मानुबन्धीनि बन्धन में डालने वाली, मनुष्यलोके मनुष्य लोक में।
अनुवाद : गुणों द्वारा पोषित इसकी शाखायें नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। इन्द्रियों के विषय कलिका (कलियाँ) हैं। नीचे मनुष्य लोक पर्यन्त इसकी जड़ें (मूल) विस्तृत हैं जो कर्म बन्धन में डालने वाली हैं।
व्याख्या : अनन्त विषय, बड़े और छोटे, जो जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक हैं, पंच महाभूतों में तीन गुणों की चेष्टा से उत्पन्न होते हैं। इस संसार-वृक्ष का पोषण तीन गुणों से होता है। इन्द्रियों के विषय इसकी कलियाँ हैं और नीचे की ओर जाने वाली मूल उन लोगों के लिए कर्मबन्धन की श्रृंखलायें हैं जो इस जगत् में आसक्ति और मोह का जीवन यापन करते हुए द्वन्द्रों (राग-द्वेष आदि) के चक्र में फंस कर उनके वश में हो जाते हैं अर्थात् अपना संयम खो बैठते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध सहित इन्द्रियों के लुभावने विषय इस विलक्षण वृक्ष के अंकुर हैं। पूर्वजन्मों की कार्मिक वृत्तियाँ जड़ें हैं जो नीचे मनुष्य लोक में विस्तार को प्राप्त हो कर कर्मों के अनुबन्ध उत्पन्न करने वाली हैं। ये जड़ें कर्मों के द्वारा बन्धन को और दृढ़ करती हैं।
मौलिक मूल अविद्या से अष्टधा प्रकृति अभिव्यक्त होती है। पाँच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार ये अष्टधा प्रकृति के अन्तर्गत हैं। वृक्ष के तने से स्वेदज, अण्डज, जरायुज और उद्भिज नामक शाखायें निकलती हैं। इनसे चौरासी लाख योनियाँ अस्तित्व में आती हैं।
एक शाखा ऊपर की ओर विकसित होती है। यह धर्म की शाखा है जो स्वर्ग में सुख-भोग प्रदान करने वाली है। अन्य शाखा वैराग्य की है जो आत्म साक्षात्कार की फलदा शाखा है। सूर्य, नक्षत्र, पितर, ऋषि-मुनि भी इस अलौकिक वृक्ष से उत्पन्न हुए हैं। इनसे ऊपर इन्द्रलोक तथा अन्य देव लोकों की शाखायें हैं। और भी ऊपर संन्यासी, तपस्वी, यतियों के लोक हैं। इससे भी और ऊपर सत्य लोक है जहाँ हिरण्यगर्भ का वास है।
मनुष्य से लेकर नीचे अचल पदार्थों पर्यन्त और उससे ऊपर ब्रह्मा के लोक तक ज्ञान और कर्म की प्रकृति के अनुरूप जो-जो भी लोक प्राप्त होते हैं वे सब संसार-वृक्ष की शाखाप्रतिशाखारूप से विस्तार हैं। वे तीन गुणों द्वारा पोषित और विकसित होते हैं जिनका आधार भौतिक जगत् है।
इन्द्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध कलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त भौतिक शरीरों की शाखाओं से प्रस्फुटित होते हैं।
इस अद्भुत संसार वृक्ष का परम मूल ब्रह्म है। गौण मूल (जड़ें) राग-द्वेष के सुप्त संस्कार हैं जो इस मर्त्यलोक में विस्तार को प्राप्त हो कर मनुष्य को शुभाशुभ कर्म में प्रेरित करके बन्धन में डालते हैं।
अब सुनो! इस वृक्ष का उन्मूलन कैसे किया जाये। इस प्रकार बताये गये ढंग से आचरण करके जो इस संसार वृक्ष को काट देता है वह इस लोक में भी सुखी रह सकता है। उसके पास सर्वोच्च ज्ञान है क्योंकि वह उस वृक्ष का द्रष्टा बन कर रहता है और जैसा यह है उसका ज्ञान रखता है। उसके बन्धन में नहीं आता।
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल-
मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।। ३ ।।
शब्दार्थ : ननहीं, रूपम् -रूप, अस्य-इसका, इह यहाँ, तथा वैसा ही, उपलभ्यते-देखा जाता है, न-नहीं, अन्तः- (इसका) अन्त, ननहीं, च-और, आदि:-आदि, न-नहीं, च-और, संप्रतिष्ठा-आश्रय, अश्वत्थम् - अश्वत्थ, एनम्-यह, सुविरूढमूलम् - दृढ़ मूलों वाले, असङ्गशस्त्रेण वैराग्य रूपी शस्त्र से, दृढेन-दृढ़ता से, छित्त्वा-काट कर ।
अनुवाद : जैसा वर्णन दिया गया वैसा स्वरूप इस संसार वृक्ष का यहाँ उपलब्ध नहीं है। न तो इसका अन्त, न आदि और न ही स्थिति देखे जा सकते हैं। वैराग्य के दृढ़ शस्त्र से इस दृढ़ मूलों वाले पीपल वृक्ष को काट कर,
व्याख्या : भाव अगले श्लोक में पूर्ण होगा।
मनुष्य जब तक अविद्या के वश में है, तब तक वह इस वृक्ष के स्वरूप, आदि, अन्त और स्थिति (मध्य) को नहीं जान सकता। हे अर्जुन, कदाचित् तुम कल्पना करोगे कि इतने विशाल वृक्ष को कैसे उखाड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है। इसे तो आँख झपकते ही, वैराग्य (अनासक्ति) की शक्तिशाली खड्ग से उखाड़ा जा सकता है।
इस वृक्ष को काट कर अन्तर्मुखी हो जाओ, आत्मा पर ध्यान करो और ईश्वर के दर्शन करो।
तथा इस प्रकार का-जैसा ऊपर वर्णन किया गया है।
क्या यह सम्भव है कि हम हवाई किले नीचे उतारें (मनोराज्य करें), अथवा खरगोश के सींग तोड़ें अथवा आकाश-कुसुम तोड़ें अथवा मगरमच्छ के दुग्ध से नवनीत प्राप्त करें अथवा पत्थर में से तेल निकालें? एवंविध, हे अर्जुन, इस संसार वृक्ष में सत्य कुछ नहीं है। अतः इसे काटा जाये अथवा नहीं, तुम इसके लिए भयभीत क्यों हो रहे हो? इस विश्व में इसका यथार्थ रूप कोई नहीं देख सकता। यह स्वप्न की वस्तु है, मृगतृष्णा का जल है, मेघों द्वारा अथवा किसी जादूगर द्वारा आकाश में रचित काल्पनिक नगर है। यह दृश्य रूप में आ कर अदृश्य हो जाता है। इस वृक्ष का द्रष्ट-नष्ट-स्वरूप है जो मृगतृष्णा के जल की भाँति है। देखते-देखते नष्ट होने वाली वस्तु द्रष्ट-नष्ट है। किसी ने अन्त नहीं देखा इस मायाविक वृक्ष का, और न ही इसका आदि और मध्य देखा है। कोई नहीं बता सकता कि यह अमुक स्थान से अथवा अमुक बिन्दु से प्रारम्भ होकर चल रहा है।
संसार-वृक्ष की मूलें अत्यन्त शक्तिशाली और गहरी हैं। इनका छेदन करने के लिए संघर्ष करना होगा ताकि यह बीज सहित अथवा गहरी मूल सहित उखाड़ा जा सके जो और मूलों को जन्म देने वाली है।
असङ्ग-वैराग्य, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा से उपरामता ।
दृढेन-बलशाली ।
तुम्हें विवेक के अभ्यास रूपी पत्थर पर वैराग्य की तलवार को तेज कर के इस वृक्ष को काटना होगा। तुम्हारा मन परमात्मा की ओर इस भाव से उन्मुख होना चाहिए कि उसी में तुम शाश्वत शान्ति प्राप्त कर सकते हो, वही एक सत्य है। इस परम आनन्द की प्राप्ति हेतु तुम्हें दृढ़ संकल्प करना होगा।
इन्द्रिय-विषयों की इच्छा सङ्ग है। इसके विपरीत, असङ्ग है। तीन प्रकार की एषणाओं (पुत्र-वित्त और लोकेष्णा) का त्याग असङ्ग है। कुल्हाड़ी जैसे वृक्ष को काटती है वैसे ही वैराग्य (असङ्ग) इस संसार वृक्ष को काटता है। इसलिए असङ्ग को खड्ग (कुल्हाड़ी) कहा गया है। संसार वृक्ष का उच्छेदन करने का अभिप्राय है इन्द्रिय-मन के संयम और असङ्ग द्वारा अहंकार, अविद्या, सुप्त संस्कार, और कर्मफल का त्याग करना। (निरूपण—VII.14)
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ।।४ ।।
शब्दार्थ : ततः तब, पदम्-लक्ष्य, तत्-वह, परिमार्गितव्यम् खोजना चाहिए, यस्मिन् -जिसमें, गताः- गये हुए, न-नहीं, निवर्तन्ति-लौटते, भूयः पुनः, तम्-उस, एव-ही, च-और, आद्यम्-आदि, पुरुषम् -पुरुष, प्रपद्ये -मैं शरण लेता हूँ, यतः जहाँ से, प्रवृत्तिः-प्रवृत्ति (आरम्भ), प्रसृता-विस्तार को प्राप्त हुई, पुराणी पुरातन ।
अनुवाद : तब वह लक्ष्य खोजना चाहिए जहाँ पहुँच कर पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात् पुनर्जन्म नहीं होता। मैं उस आदि पुरुष की शरण में हूँ जहाँ से इस सनातन प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है।
व्याख्या : सत्-चित्-आनन्द रूप से समस्त ब्रह्माण्ड को आपूरित करने वाला पुरुष है अथवा इस देह रूप पुरी में वास करने वाला पुरुष है।
सतत भगवत्-ध्यान और अनन्यमनस्क भक्ति आत्म-ज्ञान प्राप्ति के विश्वस्त साधन हैं। आदि पुरुष की शरणागत होने से उस परम पद की प्राप्ति होती है जहाँ जा कर पुनः इस संसार में लौटना नहीं पड़ता।
साधक को विष्णु के धाम का ज्ञान होना चाहिए। वहाँ पहुँचने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। आदि पुरुष की शरण में आकर इसे प्राप्त करना चाहिए। यदि साधक विष्णु के शाश्वत धाम को अथवा अनश्वर ब्राह्निक वास को जान लेता है, जिसकी महिमा और प्रकाश अक्षय्य हैं, तो पुनः वह मर्त्य लोक में नहीं लौटता।
परम पुरुष, आदि पुरुष, सच्चिदानन्द ब्रह्म ही परम लक्ष्य है। वही विष्णु धाम है। जिस प्रकार बाजीगर की माया से हाथी, घोड़े आदि मायाविक वस्तुएँ अस्तित्व में आ जाती हैं उसी प्रकार आदि मूल दिव्य शक्ति अथवा मायावी संसार वृक्ष की प्रवृत्ति उस आदि पुरुष से होती है।
उस आत्यन्तिक लक्ष्य की प्राप्ति किसे होती है? सुनो...
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-
र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ।।५ ।।
शब्दार्थ : निर्मानमोहा:-मान और मोह से विमुक्त, जितसङ्गदोषाः-संग रूप दोष को जीतने वाले, अध्यात्मनित्याः - नित्य आत्मा के विचार में निरत, विनिवृत्तकामाः समस्त कामनाएँ जिनकी मूल सहित निवृत्त हो गई हैं, द्वन्द्वैः- (सुख-दुःख आदि) द्वन्द्वों से, विमुक्ताः - मुक्त, सुखदुःखसंज्ञैः-सुख-दुःख, संज्ञक, गच्छन्ति-प्राप्त करते हैं, अमूढा:-मोह रहित, पदम् -पद (लक्ष्य), अव्ययम् शाश्वत, तत्वह ।
अनुवाद : मान और मोह जिनका नष्ट हो गया है, जो सङ्गदोष पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, जो नित्य अपनी आत्मा में ही स्थित हैं, जो आप्तकाम हो चुके हैं अर्थात् जिनकी कामनायें पूर्ण हो चुकी हैं, जो सुख-दुःख आदि द्वैतों से मुक्त हैं ऐसे (प्रकाश प्राप्त) अमूढ़ (संन्यासी) उस शाश्वत पद को प्राप्त करते हैं।
व्याख्या : जहाँ भी मान है वहाँ अहंभाव है। सत्य और असत्य में विवेक-शून्यता मोह है। वैपरीत्य मोह है, बुद्धि-लोप मोह है। सुख अथवा दुःख प्राप्त होने पर भी जो इनके सङ्ग से मुक्त रहते हैं अर्थात् सुख में झूलते नहीं और दुःख में विचलित नहीं होते वे सङ्ग दोष पर विजय प्राप्त कर चुके हैं।
कर्तव्य भाव-मैं कर्ता हूँ-यह सङ्ग है। राग-द्वेष दोष हैं। शीतोष्णता, सुख-दुःख, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा आदि विपरीत द्वन्द्व हैं। अज्ञान-अविद्या को समूल नष्ट कर के आत्म-ज्ञान प्राप्त करने वाले ही अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
अध्यात्मनित्यः - परमात्मा के विचार में सदा संलग्न ।
निवृत्तकामाः- पूर्ण रूप से समस्त कामनायें जिनकी नष्ट हो गई हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले यति अथवा संन्यासी हो जाते हैं। ज्ञान की 37sqrt(17) में समस्त इच्छायें नष्ट हो गईं। वृक्ष अग्नि की चपेट में आ जायें तो जैसे उस वृक्ष के पक्षी उड़ जाते हैं इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त पुरुष से सब कामनायें दूर चली जाती हैं।
तत्-वह लक्ष्य, जिसका वर्णन ऊपर आ चुका है।
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।।६ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, तत्-उसे, भासयते-प्रकाशित करता है, सूर्यः आदित्य, न-नहीं, शशांक:- चन्द्रमा, न-नहीं, पावकः - अग्नि, यत् जहाँ, गत्वा-जा कर, न-नहीं, निवर्तन्ते-लौटते हैं, तत्-वह, धाम- धाम, परमम् -परम, मम-मेरा ।
अनुवाद : उस तेजोमय धाम को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न ही अग्नि । जहाँ जा कर मनुष्य पुनः नहीं लौटते वही मेरा परम धाम है।
व्याख्या : वह परम धाम अपनी ही ज्योति से ज्योतित है क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। सृष्टि काल में सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि के अस्तित्व से पूर्व भी उसका अस्तित्व था। प्रलय काल में इन सब की अव्यक्त स्थिति होने पर भी उसकी सत्ता विद्यमान रहती है।
इस श्लोक का भाव कठोपनिषद् से उद्भूत है-
"वहाँ सूर्य नहीं चमकता और न ही चन्द्रमा और तारे, न ही विद्युत् वहाँ चमकती है फिर अग्नि की तो बात ही क्या! इसके प्रकाशित होने पर इसके प्रकाश से सर्वस्व प्रकाशित होता है।" (अध्याय II.5.15) यही भाव श्वेताश्वतरोपनिषद् (6.14) और मुण्डकोपनिषद् (II.2.10) में मिलता है।
सूर्य, चाँद आदि पर-ब्रह्म से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं किन्तु उस स्वयं प्रकाश ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।
धाम परमम्-परम ब्रह्म का परम उत्कृष्ट धाम। सब को प्रकाशित करने की शक्ति से युक्त सूर्य भी उस परब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता ।
“यत् धाम वैष्णवं पदं गत्वा प्राप्य न निवर्तन्ते यत् च सूर्यादिभिः न भासयते तत् धाम पदं परमं मम विष्णोः।"
"वह धाम, जहाँ से पुनरागमन नहीं होता और जिसे सूर्य, चन्द्र, सितारे, विद्युत् और अग्नि आभासित नहीं कर सकते वह परम धाम विष्णु का है ।" (निरूपण-VIII.21)
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।।७ ।।
शब्दार्थ : मम-मेरा, एव-ही, अंशः - भाग, जीवलोके जीव लोक में, जीवभूतः जीवात्मा बन कर, सनातनः सनातन, मनःषष्ठानि-जिसमें मन छठी इन्द्रिय रूप है, इन्द्रियाणि (पाँच) इन्द्रियाँ, प्रकृतिस्थानि-प्रकृति में स्थित, कर्षति आकर्षित करता है।
अनुवाद : इस जीवलोक (संसार) में मेरा अपना ही अंश जीव बन कर, प्रकृति में स्थित पाँच इन्द्रियों और छठे मन को आकर्षित करता है।
व्याख्या : अब भगवान् समझाते हैं कि व्यष्टि आत्मा अस्तित्व में कैसे आता है। जीवात्मा परमात्मा की एक किरण है। वह किरण प्रकृति में प्रवेश करती है, पाँच इन्द्रियों और मन को आकर्षित करती है और शरीर धारण कर के जीव बन जाती है। सूक्ष्म शरीर अथवा लिङ्ग शरीर स्थूल देह में कैसे प्रवेश करता है, इसका वर्णन दिया जाता है।
जल में प्रतिबिम्बित होने पर सूर्य दूषित कदापि नहीं होता । रक्त वर्ण के वस्त्र अथवा पुष्प के संयोग में स्फटिक मणि भी उसी वर्ण की प्रतीत होती है किन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं। इसी भाँति परम पुरुष जीवात्मा के कर्मों से कदापि लिप्त नहीं होता ।
अविद्या ही जीवात्मा का सीमित प्रतिबन्धक है। अविद्या-जनित सीमाओं के कारण जीवात्मा स्वयं को कर्ता और भोक्ता समझ बैठता है। सार-रूप में जीवात्मा ब्रह्म का ही एकरूप है। अविद्या-निवृत्ति होने पर सीमित प्रतिबन्ध नष्ट होता है और जीवात्मा भगवत्साक्षात्कार करता है।
घटाकाश और महाकाश में घट सीमित प्रतिबन्ध है। घट के फूटने पर घट के भीतर का आकाश बाह्य आकाश के साथ एक हो जाता है। घट यहाँ पर सीमित दीवार है इसी प्रकार जीव और ब्रह्म के मध्य अविद्या एक बाधक है। अविद्या नष्ट होने पर ज्ञान का सूर्य उदित होता है और जीवात्मा की सन्निधि प्राप्त करता है। घट के नष्ट होने पर जैसे घट का आकाश पुनः नहीं लौटता वैसे ही अन्तःकरण आदि सीमित प्रतिबन्धों के नष्ट होने पर जीवात्मा पुनः नहीं लौटता। यह ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है।
प्रतिबिम्ब, बिम्ब (विषय) का अंश मात्र है। प्रतिबिम्बित सूर्य वास्तविक सूर्य (सूर्य किरणों) का एक अंश है। जल को हटा लिया जाये तो मानो प्रतिबिम्ब भी वास्तविक सूर्य की ओर लौट जाता है। पुनः जल की ओर नहीं लौटता। इसी प्रकार अविद्या अथवा मन की निवृत्ति होने पर ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीवात्मा बिम्ब ब्रह्म में समा जाता है। इस मर्त्य लोक में उसका प्रत्यावर्तन नहीं होता।
"जीवात्मा ब्रह्म का एक काल्पनिक अंश है, सत्य नहीं। क्योंकि पर-ब्रह्म अखण्ड स्वरूप है। इसके भाग नहीं हो सकते। यदि इसके भाग हो विनाश को प्राप्त होने वाला होता हो पूर्णता भंग होती है और विनाश की स्थिति अवश्यम्भावी है।
इन्द्रियाँ प्रकृति में स्थित हैं। प्रकृति में कर्ण, त्वचा, मुख, नेत्र और नासिका में इन्द्रियों के वास स्थान निश्चित हैं। हिमालय की गुहा में वास करने बाला संन्यासी स्वप्न देखता है कि वह एक विवाहित गृहस्थ है और जीविका के लिए व्यवसाय की खोज में इतस्ततः भटक रहा है। इसी प्रकार व्यष्टि आत्मा अपनी दिव्य प्रकृति को भुला कर अपवित्र, नश्वर देह पर पवित्र अनश्वर आत्मा का अध्यास करता है और स्वयं को कर्त्ता और भोक्ता मान बैठता है। वह कल्पना करता है कि वह संसार में एक बद्ध जीव है। कभी सुखी है और कभी दुःखी है। इस प्रकार वह सीमितता के घेरे में बँध जाता है।
वस्तुतः जीव ब्रह्म से पृथक् नहीं है। मोह, कल्पना अथवा अध्यास के कारण वह ब्रह्म से पृथक् हो जाता है। मन ही वह प्रतिबन्धक है जो पार्थक्य भाव का भ्रम उत्पन्न करता है। घट के आकाश की भाँति यह जीव-ब्रह्म- भेद-भ्रान्ति का जनक है। घट के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश-महाकाश में मिल जाता है वैसे ही मन के नष्ट होने पर जीव-ब्रह्म-भेद मिट जाता है। गहन सुषुप्ति की अवस्था में मन संस्कारों और वासनाओं सहित सूक्ष्म रूप में अपने कारण मूल-अविद्या में आश्रित होता है। जाग्रत होने पर पुनः वह अविद्या की अवस्था से बाहर आ जाता है। यदि कारण (अविद्या) को ही आत्म-ज्ञान से नष्ट कर दिया जाये तो इसका कार्य रूप मन स्वयं ही नष्ट हो जाये।
जिस प्रकार मकर अपने सिर और पैरों को, जो लय की अवस्था में शरीर में थे, विस्तृत करता है, फैलाता है, उसी प्रकार जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में (अपने) मूल कारण अविद्या में स्थित अपने मन और इन्द्रियों का विस्तार करता है जिससे जाग्रतावस्था में वह विषय-भोग कर सके।
परम पुरुष की एक किरण प्रकृति में प्रवेश करती है और पाँच इन्द्रियों तथा मन को अपनी ओर आकृष्ट करती है। इस श्लोक में सूक्ष्म शरीर के स्वरूप का वर्णन है। श्रुति कहती है-
स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यः तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ।।
"वह परम पुरुष इस शरीर की सिर से पैर तक संरचना कर के जीव रूप में स्वयं उसमें प्रवेश कर गया।"
वेदान्त के अनुसार इस शरीर की रचना में उन्नीस तत्त्वों का प्रयोग होता है-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच मुख्य प्राण (प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान), मन, बुद्धि, चित्त (अवचेतन अथवा अपराचेतन मन) और अहंकार । सार रूप में, पाँच इन्द्रियाँ और मन शेष तेरह तत्त्वों की ओर भी संकेत करते हैं।
अंश-इसका अभिप्राय पृथक् किये हुए कण अथवा काटे हुए भाग से कदापि नहीं है। यह घट के आकाश की भाँति एक अंश है। आकाश के टुकड़े नहीं किये जा सकते। वह तो वही एक पूर्ण तत्त्व ही रहता है। घट की दीवार टूटने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है। (निरूपण-XIV.3)
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ।।८ ।।
शब्दार्थ : शरीरम् - शरीर, यत्-जब, अवाप्नोति-धारण करता है, यत्-जब, चऔर, अपि-भी, उत्क्रामति-उत्क्रमण (त्याग) करता है, ईश्वरः ईश्वर (जीवात्मा), गृहीत्वा-ले कर, एतानि-इन्हें, संयाति-जाता है, वायुः वायु, गन्धान् गन्ध को, इव-जैसे, आशयात् - आश्रय (पुष्पों) से।
अनुवाद : जीवात्मा जो शरीर धारण करता है उसका उत्क्रमण करते समय वह इन (इन्द्रियों और मन) को उसी प्रकार अपने साथ ले जाता है जिस प्रकार वायु अपने आश्रय स्थल (फूलों आदि) से गन्ध को साथ ले जाता है।
व्याख्या : समस्त देह का स्वामी जीवात्मा शरीर धारण करते समय इन्द्रियों और मन को अपने साथ ले कर आता है और शरीर के विघटन काल में (मृत्यु काल में) वह इन्द्रियों और मन को साथ ले जाता है जैसे वायु पुष्पों से गन्ध को ले जाता है। पुनः वह जहाँ भी जा कर जिस रूप को प्राप्त करता है वह उसी मन और इन्द्रियों के द्वारा ही कार्य करता है।
ईश्वरः जीव-शरीर आदि का स्वामी।
शरीर धारण करते समय जीवात्मा कर्ता अथवा भोक्ता प्रतीत होता है।
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।।९ ।।
शब्दार्थ : श्रोत्रम् श्रोत्र (कर्ण), चक्षुः - नेत्र, स्पर्शनम् त्वचा, च - और, रसनम् रसना, घ्राणम्-नासिका, एव - एव -ही, च-और, अधिष्ठाय-आश्रय कर के, मन: -मन, च-और, अयम् - यह (जीवात्मा), विषयान् - 3sqrt(34) के विषयों को, उपसेवते -भोगता है।
अनुवाद : यह (जीवात्मा) कर्ण, नेत्र, त्वचा, रसना, घ्राण और मन के आश्रित होकर इन्द्रियों के विषयों का उपभोग करता है।
व्याख्या : सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में वास कर के किस प्रकार विषयों का सेवन करता है-इसका वर्णन किया जाता है।
जीवात्मा इन्द्रियों सहित मन का आश्रय लेकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इन विषयों का सेवन करता है।
मन रूपी अद्भुत कार (वाहन) पर सवार हो कर श्रोत्र के द्वार से पलक झपकते ही यह दौड़ पड़ता है और संसार के विविध संगीत का आनन्द लेता है। संवेदनशीन शिराओं को पकड़ कर यह स्पर्श तन्मात्रा के राज्य में प्रवेश करता है और त्वचा के रोम कूपों के माध्यम से कोमल विविध विषयों का सुख लेता है। सुन्दर सुन्दर पर्वत शिखरों पर आरोहण कर के चक्षु द्वार से सौन्दर्यशील रूपों का सेवन करता है। मुख रूपी गुहा में प्रवेश हो कर रसनेन्द्रिय का आश्रय ले कर यह सुस्वादु, सरस खाद्य पदार्थों का सेवन करता है। नासिका द्वार से सुगन्ध वन में पहुँच कर मन भर कर सुगन्ध ग्रहण करता है।
कर्ण, चक्षु, त्वचा, रसना, नासिका और मन में अपना वास बना कर यह जीवात्मा विषय-वासनाओं का भोग करता है। मन, बुद्धि, अवचेतन मन, अहंकार, दस इन्द्रियाँ और पाँच प्राणों की सहायता से यह बाह्य जगत् के अनुभव लेता है।
घ्राणमेव च-च (और) शब्द इस बात का संकेत देता है कि हमें पाँच कर्मेन्द्रियाँ और अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) का भी समावेश करना है।
कठोपनिषद् में कहा है-"आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः", इन्द्रियाँ, मन और आत्मा संयुक्त रूप से भोक्ता कहलाते हैं, ऐसा विद्वानों का कथन है। (निरूपण - V.15-29; IX.24; XIII.21-32)
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।।१०।।
शब्दार्थ : उत्क्रामन्तम् - (शरीर) त्यागते हुए को, स्थितम् -स्थित रहते हुए को, वा-अथवा, अपि-भी, भुञ्जानम् -भोग करते हुए को, वा-अथवा, गुणान्वितम् - गुणों से संयुक्त हुए को, विमूढाः-अज्ञानी जन, न-नहीं, अनुपश्यन्ति-देखते, पश्यन्ति-देखते हैं, ज्ञानचक्षुषः- ज्ञान रूप नेत्रों वाले ।
अनुवाद : अज्ञानी जन उस जीवात्मा को शरीर त्यागते हुए, (शरीर में) स्थित हुए, भोग करते हुए अथवा तीन गुणों से युक्त हुआ नहीं देखते । किन्तु जिनके पास ज्ञान चक्षु हैं वे ज्ञानी जन उसे देखते हैं।
व्याख्या : यद्यपि आत्मा मनुष्य के अत्यन्त समीप है और सुगमता से उसकी चेतना के क्षेत्र में आ सकता है किन्तु विमूढ़ और भ्रान्त जन उसे देखने में असमर्थ हैं क्योंकि वे प्रकृति के गुणों के आधीन हैं, उनके मन अनवरत रूप से इन्द्रिय-विषयों में भटकते रहते हैं और मोह जाल में फंस जाते हैं, वे शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं और उनकी दृष्टि बाह्य रूपों में अटक कर रह जाती है। किन्तु अन्तर्चक्षु जिनके खुल चुके हैं वे उसे देख सकते हैं।
यम ने नचिकेता से कहा - "स्वयंभू ब्रह्म ने इन्द्रियों को बहिर्गामी बनाया। इसलिए मनुष्य बाह्य जगत् देखता है भीतर का नहीं।" आगे वे कहते हैं-"किन्तु अमृतत्व के इच्छुक विद्वज्जन विषयों से पराङ्मुख हो कर दृष्टि अन्तर्मुखी कर के भीतर आत्मा के दर्शन करते हैं।" कठोपनिषद् (IV.1)
ज्ञानी जन ज्ञान-चक्षु से जान लेते हैं कि आत्मा शरीर से सर्वथा पृथक् है। वे शरीर से पृथक् आत्मा के अस्तित्व का अनुभव कर के जान लेते हैं कि चुम्बक के समक्ष लौह खण्ड की भाँति, आत्मा के समक्ष शरीर चेष्टा करता है।
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ।।११ ।।
शब्दार्थ : यतन्तः- (पूर्णत्व की प्राप्ति हेतु) यत्न करते हुए, योगिनः-योगी जन, च-और, एनम्-इसे, पश्यन्ति-देखते हैं, आत्मनि-आत्मा में, अवस्थितम् -स्थित, यतन्तः-यत्न करते हुए, अपि -भी , अकृतात्मानः - अशुद्धचित्त वाले, न नहीं, एनम्-इसे, पश्यन्ति-देखते हैं, अचेतसः- अज्ञानी ।
अनुवाद : पूर्णत्व प्राप्ति हेतु यत्न करते हुए योगी जन उसे आत्मा में स्थित देखते हैं किन्तु अशुद्ध चित्त वाले और अज्ञानी जन यत्न करने पर भी उसे देख नहीं पाते।
व्याख्या : जीवात्मा का, उद्भव सम्बन्धी वर्णन पूर्ण हुआ।
लौह (दृढ़) निश्चय से, आग्नेय संकल्प से, निष्ठा से, उद्यम और समाहित चित्त से योगी जन अपने हृदयों में उसे स्थित देखते हैं। वे अपने ही मन-बुद्धि में उसे अवस्थित देखते हैं। वे उसे इस प्रकार पहचानते हैं- “यह मैं हूँ"। किन्तु मूढ़ बुद्धि, चंचल मन और इन्द्रियों वाले मनुष्य जो तपश्चर्या, निःस्वार्थ सेवा और दान से विशुद्ध नहीं हुए, जिनका मन संयत नहीं है, जिन्होंने सतत ध्यान का अभ्यास नहीं किया है, अपने अशुभ कर्मों का त्याग नहीं किया है, काम, अभिमान, दम्भ, क्रोध, लोभ, उद्दण्डता का निराकरण नहीं किया है, वे शास्त्राध्ययन आदि द्वारा कितना ही संघर्ष क्यों न कर लें, उसे देख नहीं सकते। वे आत्म-साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं। अशुद्ध मन वाला यदि शास्त्रों के अध्ययन से आत्म-प्रकाश पाना चाहे तो सर्वथा असम्भव है। साधक का मन शान्त और एकाग्र होना चाहिए। उसे आत्मा पर अनवरत रूप से दृढ़ता पूर्वक ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। केवल तभी वह उस परम आत्म तत्त्व को अपने हृदय में अवस्थित देख सकता है, उसका अभिज्ञान कर सकता है और साक्षात्कार कर सकता है।
भौतिक जगत् के अनुभवों का सार रूप केवल वही एक परम पुरुष है जिसे, अग्नि, विद्युत्, सूर्य और चन्द्रमा आभासित नहीं कर सकते, जिसे प्राप्त हो कर ज्ञानी जन पुनः इस संसार में नहीं लौटते, जन्म-मृत्यु के बन्धन में नहीं पड़ते, ये मानव समुदाय जिसका एक काल्पनिक भाग है जो घटाकाश की भाँति अविद्यावश ऐसा सत्य प्रतिभासित हो रहा है।
जिस प्रकार घट फूटने पर घटाकाश महाकाश के साथ एक हो जाता है उसी प्रकार उपनिषदों के महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि', 'तत्त्वमसि' के यथार्थ अर्थ का ज्ञान होने पर इन वाक्यों पर अनवरत ध्यान से प्राप्त आत्म-ज्ञान के द्वारा
अविद्या नाश से जीवात्मा परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। इस तादात्म्यता की स्थिति प्राप्त होने पर ज्ञानी विचार करता है कि समस्त अनुभूतियों का अवलम्ब और सार केवल वही परमात्मा है।
अर्जुन को यह ज्ञान कराने के लिए भगवान् आगामी चार श्लोकों में अपनी अभिव्यक्तियों का सारांश देते हैं।
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ।।१२।।
शब्दार्थ : यत्-जो, आदित्यगतम् सूर्य में, तेजः-तेज, जगत् जगत्, भासयते-प्रकाशित करता है, अखिलम् समस्त, यत्-जो, चन्द्रमसि-चन्द्रमा में, यत्-जो, च-और, अग्नौ-अग्नि में, तत्-वह, तेजः-प्रकाश, विद्धि-जानो, मामकम् -मेरा ।
अनुवाद : संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य का आलोक तथा चन्द्र और अग्नि में विद्यमान तेज-यह सब मेरा ही जानो ।
व्याख्या : इस श्लोक में भगवान् की महिमा का गुणगान उनकी सर्वप्रकाशक आलोक चेतना के रूप में किया गया है।
मैं संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य के आलोक का कारण और स्रोत हूँ। चन्द्र और अग्नि में प्रतिभासित सूर्य के आलोक का कारण भी मैं ही हूँ।
तेजः-प्रकाश । चेतना का प्रकाश ।
यदि ऐसा है तो एक आलोचक कहता है-"सूर्य का प्रकाश चराचर समस्त पदार्थों में समान रूप से रहता है तो भगवान् ने प्रकाश के इस विशेष गुण की विद्यमानता सूर्य, चांद और अग्नि में ही विशेष क्यों कही है?" उत्तर है-"चेतना के प्रकाश की उच्चतर अभिव्यक्ति सूर्यादि में उनमें विराजित सत्त्व पुंज की अधिकता के कारण है। उनमें सत्त्व अत्यन्त देदीप्यमान् और प्रकाशमान् है। इसी कारण से तेज का यह विशेष गुण उनमें निहित कहा गया है।"
एक अन्य चित्रण इस प्रकार है-मनुष्य की मुखाकृति दीवार में, काष्ठ खण्ड में अथवा प्रस्तर खण्ड में प्रतिबिम्बित नहीं होती किन्तु वही आकृति एक निर्मल दर्पण में अत्यन्त सुन्दर रूप से प्रतिबिम्बित होती है। दर्पण में प्रतिबिम्ब की स्पष्टता का स्तर, दर्पण के पारदर्शी स्तर पर अवलम्बित है। दर्पण जितना अधिक पारदर्शी होगा, मुख का प्रतिबिम्ब उतना ही स्पष्ट होगा। इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश सूर्य में और भक्त के परिमार्जित हृदय में आलोकित होता है।
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।।१३ ।।
शब्दार्थ : गाम् -पृथ्वी, आविश्य-प्रवेश कर के, च-और, भूतानि-प्राणियों को, धारयामि धारण करता हूँ, अहम् -मैं, ओजसा अपनी शक्ति से, पुष्णामि-पोषण करता हूँ, च-और, औषधीः वनस्पतियां, सर्वाः सब, सोमः- चन्द्रमा, भूत्वा हो कर, रसात्मकः - अमृतमय ।
अनुवाद : पृथ्वी में प्रवेश कर के मैं ही अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ, रसमय चन्द्रमा बन कर समस्त औषधियों (वनस्पतियों) को पुष्ट करता हूँ।
व्याख्या : इस श्लोक में जगत् नियन्ता (पालनकर्ता) ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है।
ओजस् -ईश्वर की शक्ति । विस्तृत स्वर्ग और धरती इसी शक्ति पर आलम्बित हैं। यह शक्ति पृथ्वी में प्रवेश कर के जगत् का पालन करती है। आसक्ति और मोह से यह शक्ति शून्य है। ईश्वरीय शक्ति पर आश्रित होने के कारण यह धरती न तो गिरती है, न खण्डों में विभाजित होती है और न ही अन्य लोकों में विलीन होती है।
प्रवेशन द्वारा ईश्वर चर और अचर समस्त पदार्थों को शक्ति प्रदान करता है।
रसात्मकः सोमः - रसमय सोम (चन्द्र) । चन्द्रमा सब रसों का भण्डार माना जाता है। मैं अमृतमय चन्द्रमा बन कर सब औषधियों, वनस्पतियों जैसे धान, गेहूँ आदि का पोषण करता हूँ, उनमें रस और स्वाद भरता हूँ। मैं अपने ओजस् के द्वारा वनस्पति जगत् को पुष्ट करता हूँ जो मिट्टी में फैल कर (प्रवेश करके) मधुर रस अथवा पेड़-पौधों और औषधियों में स्वाद भरता है। रसयुक्त चन्द्रमा, सब पौधों और वनस्पतियों में रस और स्वाद भर कर उनका पोषण करता है।
और भी-
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ।।१४ ।।
शब्दार्थ : अहम् -मैं, वैश्वानरः- वैश्वानर (अग्नि), भूत्वा हो कर, प्राणिनाम् -प्राणियों के, देहम्-देह (में), आश्रितः - आश्रित, प्राणापानसमायुक्तः प्राण और अपान से युक्त हो कर, पचामि पचाता हूँ, अन्नम् अन्न को, चतुर्विधम् - चार प्रकार के।
अनुवाद : वैश्वानर अग्नि (जठराग्नि) बन कर मैं प्राणियों के देह में स्थित हो कर प्राण और अपान की सहायता से चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ।
व्याख्या : समस्त प्राणियों में जठराग्नि के रूप में ईश्वर की अन्तस्थिति यहाँ वर्णित है।
वैश्वानर-उदरीय अग्नि । श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया से यह अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्याप्त परिमाण में भोजन इस सतत प्रक्रिया से पचता है। वैश्वानर अग्नि बन कर उदर रूपी अद्भुत लेबोरेटरी (laboratory) में प्रवेश कर के मैं भोजन को पचाता हूँ।
अन्नं चतुर्विधम् -
(१) चबा कर खाने योग्य-भक्ष्यम् (रोटी आदि)
(२) निगल कर ग्रहण करने योग्य भोजन-भोज्यम् (दूध आदि)
(३) चाट कर लेने वाला भोजन-लेह्यम् (चटनी)
(४) चूसा जाने वाला भोजन-चोष्यम् (ईख आदि)
एक अन्य वर्गीकरण एवंविध है-
(१) चावल, पृथ्वी-अन्नम् (स्थूल भोजन है) मनुष्यों के लिए
(२) जल, आप्यन्नम् (जलीय भोजन) चातक आदि पक्षियों के लिए
(३) अग्नि, तेजसन्नम (उष्ण भोजन) विशेष जीवों के लिए
(४) वायु, वाय्वन्नम् (वायव्य भोजन) सर्प आदि के लिए
अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषः येनेदमन्नं पच्यते।।
"यह अग्नि जो मनुष्य में विद्यमान है और जिससे अन्न पचाया जाता है-वैश्वानर अग्नि है।" (बृहदारण्यकोपनिषद् - 4.8 * 0.8 )
जो मनुष्य यह सोचता है, ध्यान करता है अथवा अनुभव करता है कि वैश्वानर अग्नि भोक्ता है, अग्नि द्वारा भुक्त भोजन सोम (चन्द्रमा) है और दोनों संयुक्त हो कर अग्नि-सोम बनाते है, वह भोजन की अशुद्धताओं से दूषित नहीं होता। भोजन करने से पूर्व जो व्यक्ति ध्यानस्थ हो कर विचार करता है कि भोक्ता और भोग्य रूप में यह समस्त संसार अग्नि और सोम से बना हुआ है, वह अशुद्ध भोजन से उत्पन्न होने वाली बुराई से लिप्त नहीं होता ।
भोजन करने से पूर्व इस श्लोक का जप करने से तुम भोजन में अशुद्धता के पाप से मुक्त हो जाओगे ।
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ।।१५ ।।
शब्दार्थ : सर्वस्य-सब का, च-और, अहम् -मैं, हृदि-हृदय में, सन्निविष्टः-स्थित, मत्तः मुझ से, स्मृतिः-स्मृति, ज्ञानम्-ज्ञान, अपोहनम् -हास (स्मृति और ज्ञान का), च-और, वेदैः- वेदों के द्वारा, च-और, सर्वैः सब (के द्वारा), अहम् -मैं, एव-ही, वेद्यः- जानने योग्य, वेदान्तकृत् वेदान्त का रचनाकार, वेदविद्-वेदों का ज्ञाता, एव-ही, च-और, अहम् मैं।
अनुवाद : (अन्तर्यामी रूप से) सब के हृदयों में मैं स्थित हूँ, मुझ से ही स्मृति और ज्ञान एवम् उनका हास है। वेदों के द्वारा ज्ञातव्य तत्त्व मैं ही हूँ। मैं ही वेदान्त का प्रणेता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ।
व्याख्या : सब चेतन प्राणियों के हृदयों में अन्तर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ। सब प्राणियों के आत्म रूप मुझ से स्मृति, ज्ञान और उनका हास है। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप पुरुष स्मृति और ज्ञान से समन्वित होते हैं। अशुभ कर्मों के फलस्वरूप असाधुपुरुष स्मृति और ज्ञान से शून्य होते हैं। सद्गुणों से शान्ति मिलती है और इसीलिए बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है।
अपोहनम् -विनाश, हास, शून्यता अर्थात् ज्ञान और स्मृति का हास और 'तर्क शक्ति' का भी विनाश । काम, क्रोध, लोभ और मोह तथा शोक से स्मृति और ज्ञान का विनाश होता है।
स्मृति-स्मरण शक्ति । यह अन्तःकरण की एक विशेष वृत्ति है जो संस्कार-जनित है और सांसारिक मनुष्य को, जिसने योग का अभ्यास न किया हो, इस जीवन में पूर्व कृत् भोगों और इन्द्रिय-विषयों का स्मरण कराती है। योगी को अपने पूर्व जन्मों के उस भावातीत ज्ञान की पुनर्चेतना होती है जो ज्ञान देश-काल-कारणत्व और दृश्य प्रकृति से अतीत होता है।
मैं ही वेदों का प्रमुख विषय हूँ। वेदों को समझने का अभिप्राय मुझे समझना है। सब वेदों में मैं ही एक परम पुरुष जानने योग्य हूँ। यह 'मैं' हूँ जो वेदोपदेश और वेदार्थ को जानता है। वेदों से भी परे उपनिषदों का मैं लेखक हूँ जो वेदान्त हैं और नाम-रूप-गुण से अतीत उस परम पुरुष का ज्ञान है।
भगवान् नारायण के गुणों का संक्षिप्त वर्णन इन अभिव्यक्त वाहन विशेष चार श्लोकों के माध्यम से किया गया है। अगले श्लोक से सब प्रकार के प्रतिबन्धों से अतीत पुरुषोत्तम के स्वरूप का विशद वर्णन दिया गया है। (निरूपण - X.20)
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।।१६ ।।
शब्दार्थ : द्वौ दो, इमौ-ये, पुरुषौ-पुरुष (जीव), लोके संसार में, क्षरः नश्वर, च-और, अक्षरः-अनश्वर, एव-ही, च-और, क्षरः नश्वर, सर्वाणि समस्त, भूतानि-जीव, कूटस्थः-अव्यय (निर्विकार), अक्षरः- अनश्वर, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : इस लोक में क्षर और अक्षर भाव से दो पुरुष हैं। क्षीण होने वाले नश्वर-क्षर पुरुष हैं और इसके विपरीत अक्षर पुरुष हैं।
व्याख्या : अब भगवान् दिव्य सत्ता के तीन पक्षों का वर्णन करते हैं। एक तो जीवात्मा है जो नश्वर है, द्वितीय भगवान् की माया शक्ति जो अविनाशी है और तृतीय है पुरुषोत्तम अथवा परम पुरुष ।
विकार को प्राप्त होने वाला, यह सम्पूर्ण परिवर्तशील संसार नश्वर है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त, सब चेतन और जड़ (चराचर) पदार्थ, वह सब, मन जिसकी कल्पना कर सकता है, पंचभूतों से निर्मित सब पदार्थ, वह सब जो विकारी है, जो नाम और रूप से युक्त है, जो खुले नेत्रों से दर्शनीय है, तेरहवें (त्रयोदश) अध्याय में जिसका शरीर और क्षेत्र के विकार-वृत्तियों के रूप में वर्णन किया गया-सब क्षर है, नश्वर है। परिवर्तनशील ही क्षर है। यह पदार्थ का नित्य परिवर्तित होने वाला स्वरूप है जो जड़ है, अचेतन है। अक्षर अपरिवर्तनशील अविकारी है।
संसार में 'पुरुष' संज्ञा से अभिहित, जीवों के दो पृथक् विभाग हैं क्योंकि वे परम पुरुष के सीमित प्रतिबन्धक हैं। नश्वर प्राणियों का उद्भव भगवान् की माया शक्ति से है जो बीज रूप में रहती है। विभिन्न नश्वर जीवों के कर्म और सुषुप्त संस्कारों का वास स्थान यही मूल प्रकृति है। माया शक्ति अक्षर पुरुष है। अव्यक्तावस्था प्रायः सुषुप्ति अथवा गहन अविद्या की अवस्था कही जाती है क्योंकि उस समय न तो चेतना और न ही अचेतना रहती है।
यह केवल संभावित अवस्था होती है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें जीवन के सम्पूर्ण रूप अपनी सुप्त सीमाओं सहित, फल के बीज में पड़े सुप्त वृक्ष की भाँति विद्यमान रहते हैं। इस अवस्था में पदार्थ और ऊर्जा एक ही होते हैं। इस अवस्था में शब्द, पदार्थ और ऊर्जा अभिन्न रूप में वर्तमान रहते हैं। इस अवस्था में गुण साम्यावस्था में रहते हैं।
अविनाशी को कूटस्थ कहते हैं अर्थात् जो अचल पिंड की भाँति पड़ा रहता है। सब प्राणियों के मूल (कूट) में जो स्थित है वह कूटस्थ है। कूट को माया के अर्थ में ले सकते हैं और तब कूटस्थ का अभिप्राय होगा जो स्वयं को माया के अनेक रूपों में प्रकट करता है। माया अथवा कूट सत्य को आवृत करने वाले, मिथ्या दर्शाने वाले और सांसारिक मनुष्यों को धोखे (भ्रान्ति) में रखने वाले हैं। आवरण-विक्षेप-शक्ति (veiling and vacillating power) कूटस्थ है। क्योंकि माया शक्ति को आत्म-ज्ञान के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता, इसी कारण यह अनन्त है। इसी कारण से इसे अक्षर भी कहते हैं। संसार के बीज का कोई अन्त नहीं है अतः इसे इस भाव में अनश्वर कहते हैं कि
आत्म-ज्ञान की अविद्यमानता में भी यह नष्ट नहीं होता, किन्तु ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर बीज पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। भ्रान्ति का निवारण होता है और प्रत्येक वस्तु एक वैश्विक चेतना के रूप में दृष्टिगत होती है। पदार्थ का केवल माया का आवरण नष्ट किया जाता है।
पुरुषोत्तम अथवा सर्वोच्च उत्कृष्ट सत्ता पुरुष इन दोनों से पृथक् है। वह नश्वर और अनश्वर इन दोनों से अतीत है। वह इन नश्वर और अनश्वर सीमित प्रतिबन्धकों की बुराई से प्रभावित नहीं होता। वह शाश्वत है, पवित्र है, चेतन स्वरूप है और स्वभाव से ही नित्य मुक्त है।
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ।।१७ ।।
शब्दार्थ : उत्तमः उत्तम, पुरुषः-पुरुष, तु-लेकिन, अन्यः-अन्य, परमात्मा-परमात्मा, इति-इस प्रकार, उदाहृतः-कहा जाता है, यः जो, लोकत्रयम् तीनों लोकों को, आविश्य-व्याप्त हो कर, बिभर्ति - धारण करता है, अव्ययः-अविनाशी, ईश्वरः ईश्वर ।
अनुवाद : किन्तु उत्तम पुरुष अन्य है जो तीनों लोकों में व्याप्त हो कर उनका पोषण करता है और जिसे परमात्मा, अविनाशी, ईश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है।
व्याख्या : तीनों लोकों में व्याप्त हो कर भी पुरुषोत्तम ब्रह्माण्ड से परे है। इसलिए इस लोक के मनुष्य और वेद उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। वह तीन लोकों में व्याप्त हो कर उन्हें धारण करता है । पुनरपि वह संसार में लिप्त नहीं होता। वह संसार से अथवा सांसारिकता से ऊपर है।
जिस प्रकार जाग्रतावस्था, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं से पृथक् है, सूर्य मण्डल अपनी किरणों से और मरीचिका से (जिसका कारण किरणें हैं) से पृथक् है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम नश्वर और अनश्वर पुरुष से पृथक् है।
पुरुषोत्तम शान्ति का संश्रय है। उसी में सब प्राणी आश्रय और शाश्वत विश्राम लेते हैं। वह अनुपमेय है क्योंकि वह स्वयं में स्थित है। उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। स्वयं उसी से ही उसकी उपमा दी जा सकती है-वह उपमान भी है और उपमेय भी है। अव्यक्त और अक्षर ब्रह्म, जो लोकातीत है, मूलतः पुरुषोत्तम ही है जो क्षर और अक्षर दोनों से अतीत है।
पुरुषोत्तम, क्षर और अक्षर से सर्वथा पृथक् है। वह परम पुरुष है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी 'आत्मा' कहे जाते हैं किन्तु ये गौण आत्मायें हैं। परमात्मा, आदि आत्मा है। पुरुषोत्तम अथवा परमात्मा अविद्या जनित अन्य आत्माओं की अपेक्षा परम, सर्वोच्च और उत्कृष्ट है। वह अन्तर्यामी रूप से सब प्राणियों में विराजित है। प्राणियों की अन्तर्निहित चेतना वही है। वह सब का आधार है। वह नियन्ता है, अन्तः-शासक है। वह स्वतन्त्र है, आत्म निर्भर है, इसलिए वेदान्त में उसे परमात्मा कहते हैं।
अन्यः-अन्य, अन्य दो से सर्वथा पृथक् ।
लोकत्रयम् -तीन लोक-भूः (पृथ्वी), भुवः (अन्तरिक्ष), स्वः (स्वर्ग) -ये तीन लोक हैं।
पुरुषोत्तम का और अधिक वर्णन इस प्रकार है-
वह अविनाशी है, सर्वज्ञ भगवान् नारायण हैं जो अपनी प्राणभूत शक्ति से तीनों लोकों में व्याप्त रहता है और मात्र अपनी सत्ता से उनका धारण-पोषण करता है।
अव्यय-अनश्वर । जो जन्म-मृत्यु आदि विकारों से रहित है। एक राजा जिस प्रकार प्रजा पर शासन करते हुए, उन्हें वश में रखते हुए उनसे पृथक् रहता है उसी प्रकार परमात्मा, जो नश्वर और अनश्वर पदार्थों का शासक है, उनसे पृथक् है। (निरूपण-VIII.20)
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।।१८ ।।
शब्दार्थ : यस्मात् -जिस से, क्षरम्नश्वर, अतीतः अतीत, अहम् -मैं, अक्षरात् - अनश्वर से, अपि-भी, च-और, उत्तमः- उत्तम, अतः इसलिए, अस्मिㅡ(मैं) हूँ, लोके-लोक में, वेदे वेदों में, च-और, प्रथितः घोषित, पुरुषोत्तमः परम पुरुष ।
अनुवाद : क्योंकि मैं नश्वर जगत् से अतीत हूँ और अनश्वर से भी उत्तम हूँ, मुझे लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम कहा जाता है।
व्याख्या : पुरुषोत्तम भगवान् का सर्वविदित नाम है। उचित ही है यह नाम, क्योंकि वह उत्तम पुरुष है।
क्षर-नश्वर संसार रूपी वृक्ष ।
अक्षर-अनश्वर । संसार-वृक्ष का बीज ।
क्योंकि मैं मिथ्या नश्वर संसार-वृक्ष से परे हूँ और अनश्वर (बीज रूप में संसार वृक्ष) से भी अति उत्तम (अत्युत्तम) हूँ और इस प्रकार नश्वर (क्षर) और अनश्वर (अक्षर) इन दोनों से अतीत हूँ, लोक में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्त इसी नाम से मुझे जानते हैं। कवि भी इस नाम से मेरा वर्णन करते हैं।
मैं सब प्रकार की सीमाओं से अतीत हूँ। मुझमें द्वैत का कोई लक्षण नहीं है, इसीलिए वेद और लोक मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं।
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ।।१९ ।।
शब्दार्थ : यः जो, माम् -मुझे, एवम् - इस प्रकार, असंमूढः- ज्ञानी पुरुष, जानाति जानता है, पुरुषोत्तमम् -पुरुषोत्तम को, सः-वह, सर्ववित् - सर्वज्ञ, भजति-पूजा करता है, माम् -मेरी, सर्वभावेन-हृदय से, भारत- हे भारत ।
अनुवाद : जो ज्ञानी पुरुष मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप में जानता है वह सर्वज्ञ सर्वभाव से, हे अर्जुन, मुझे ही भजता है।
व्याख्या : आत्म-ज्ञान की महिमा इस श्लोक में वर्णित है।
असम्मूढः-अभ्रान्त, ज्ञानी, मोह से मुक्त। भ्रम रहित मनुष्य भौतिक शरीर और आत्मा का एकीभाव नहीं देखता। वह शरीर, प्राण, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि और कारण शरीर को अपना आत्म-स्वरूप नहीं समझता क्योंकि वह तो अपने मूल सत्-चित्-स्वरूप में अवस्थित रहता है और ब्रह्म के साथ तादात्म्य भाव रखता है।
वही साधक ज्ञानी है जो यह जानता है कि श्रीकृष्ण कोई मनुष्य नहीं हैं, वे पुरुषोत्तम हैं, परम पुरुष हैं। ऐसा भक्त ही पूर्ण हृदय से उन्हें भजता है। वही सर्वविद् है, सर्वज्ञ है। वह जानता है कि भगवान् कृष्ण सब प्राणियों के अन्तरात्मा हैं। वह अनेक में एक और एक में अनेक देखता है। उसके लिए कोई ऊँचा-नीचा नहीं, दुःख-सुख नहीं, अच्छा-बुरा नहीं, गुण-अवगुण नहीं, राग-द्वेष नहीं। वह समस्त द्वैतों से अतीत है।
माम् -मुझे अर्थात् भगवान् को, जिनका वर्णन ऊपर आया है। सर्ववित्-जो विस्तार से सब प्रकार का ज्ञान रखता है।
जानाति-जानता है कि "मैं वह हूँ"।
सर्वभाषेन-सम्पूर्ण हृदय से, अन्तरात्मा से, सहृदयेन, अपना सम्पूर्ण विचार पूर्ण रूप से सब की आत्मा-परमात्मा में नियुक्त; परमात्मा में पूर्ण मन से, अनन्य भाव से केन्द्रित ।
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।।२० ।।
शब्दार्थ : इति-इस प्रकार, गुह्यतमम् - अत्यन्त गोपनीय, शास्त्रम् - विज्ञान, शास्त्र (शिक्षा), इदम् - यह, उक्तम्-कहा गया, मया-मेरे द्वारा, अनघ-निष्पाप (अर्जुन), एतद्बुद्ध्वा-इसे जान कर, बुद्धिमान् बुद्धिमान, स्यात् -हो जायेगा, कृतकृत्यः-कृतार्थ, च-और, भारत-हे भारत ।
अनुवाद : हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसका ज्ञान प्राप्त कर के मनुष्य बुद्धिमान् और कृतार्थ हो जाता है।
व्याख्या : गुह्यतमम् - अत्यन्त रहस्यपूर्ण ।
बुद्धिमान् यहाँ इसका अभिप्राय आत्म-ज्ञानी से है।
इस श्लोक में आत्म-ज्ञान की प्रशंसा की गई है जिसकी प्राप्ति जन्म-मृत्यु और कर्म के बन्धन काटने वाली है। इस मार्मिक तत्त्व ज्ञान को यथार्थ रूप में समझने वाला मनुष्य बुद्धिमान् बनता है और आत्म-ज्योति प्राप्त करता है। इसके उपरान्त उसे कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रह जाती न ही
कुछ ज्ञेय शेष रह जाता है। मानवीय अस्तित्व का अथवा जीवन का लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाता है। उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। आत्म साक्षात्कार के लिए उसका संघर्ष, उसका उद्यम अवसान को प्राप्त होता है। वह पूर्णत्व की प्राप्ति कर लेता है। उसे परमात्मा का पूर्ण ज्ञान मिल गया है। वह ब्रह्म ज्ञानी हो गया है। वह दिव्य चेतना में चेष्टा (गति) करता है। सर्वत्र आत्म तत्त्व के दर्शन करता है। ब्रह्म में वास करता है। समस्त प्रक्रियाओं को अब वह दैवी क्रीड़ा समझता है, दिव्य लीला मानता है।
ब्रह्म ज्ञान होने पर जीवन के समस्त कर्त्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। कर्म बन्धन से मोक्ष मिलता है। आत्म ज्ञानी, जीवन्मुक्त अथवा प्रकाश प्राप्त संन्यासी हो जाता है जिसने देह चेतना का अतिक्रमण कर लिया हो, जो तीन गुणों से अतीत हो गया हो, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति-इन तीन अवस्थाओं से ऊपर उठ गया हो, राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों से मुक्त हो कर जन्म-मृत्यु के बन्धन से भी मोक्ष पा लिया हो। ऐसा ज्ञानी भली प्रकार जानता है कि उसकी पुनर्जन्म की श्रृंखला नष्ट हो चुकी है, कर्तव्य कर्म पूर्ण हो चुका है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो चुका है और अब उसे और कुछ करना अथवा सीखना शेष नहीं रहा । उसने जीवन के गहन रहस्य को जान लिया है-ब्रह्माण्ड की प्रहेलिका सुलझ गई है। अब वह सर्ववित् है।
सम्पूर्ण गीता एक विज्ञान कही जाती है। उसमें भी पञ्चदश अध्याय का उपदेश स्तवन हेतु उत्कृष्ट माना गया है। इस अध्याय में सम्पूर्ण गीता, उपनिषद् और वेदों का सार निहित है। यह वेदों के दुग्ध से प्रमथित नवनीत है। ऐसा वर्णित है कि पीपल वृक्ष का ज्ञान करने वाला वेदों का ज्ञाता है (XV.1)। भगवान् ने यह भी कहा - ''वेदों के द्वारा जानने योग्य तत्त्व मैं ही हूँ" (XV.15) । ऊपर वर्णित ढंग से जो मनुष्य इस विज्ञान को जान लेता है वही बुद्धिमान् है, अन्य नहीं। उच्च ब्राह्मण जाति में जन्म लेने पर जो भी कर्त्तव्य कर्म विहित हैं वे सब आत्म-ज्ञान की प्राप्ति में सम्पूर्ण हो जाते हैं। “आत्यन्तिक रूप में समस्त कर्मों का अवसान ज्ञान में होता है ।'' (IV .33) यह जन्म की, विशेष रूप से ब्राह्मण कुल में जन्म की सफलता है, पूर्णता है क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त कर के ही द्विज अपने कर्त्तव्य कर्म पूर्ण करता है अन्यथा नहीं, ऐसा मनुस्मृति में निर्दिष्ट है।
तुमने परमात्मा के विषय में इस सत्य को मुझसे सुना है, तुम अत्यन्त सौभाग्यशाली हो, तुमने अपने सब कर्त्तव्य पूर्ण कर लिए है और अब तुम आत्म-ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो।
अनघ और भारत-इन शब्दों का प्रयोग कर के भगवान् कृष्ण संकेत देते हैं कि जब कोई सामान्य व्यक्ति भी इस पञ्चदश अध्याय को जान कर, ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कृतकृत्य हो सकता है तो अर्जुन का तो कहना ही क्या, जो अनघ (पाप रहित) था और जिसने दिव्य गुणों सहित उच्च कुल में जन्म लिया था।
अनघ शब्द को प्रयोग कर के भगवान् यह तथ्य भी परिलक्षित करते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु को यह अत्यन्त गोपनीय ज्ञान केवल गुण संपन्न योग्य साधकों को ही प्रदान करना चाहिए जो शुद्ध-हृदय हों, संयत हों, शान्त हों और मोक्ष हेतु साधन चतुष्टय से युक्त हों (III.3) । अशुद्ध मन सत्य को ग्रहण करने में शक्य नहीं होता । पापी मनुष्य अपनी विक्षिप्त बुद्धि से सत्य को भी विकृत कर देगा और इस प्रकार अपने और शिष्यों के विनाश का कारण बनेगा।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।।१५ ।।
।। इति पुरुषोत्तमयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ षोडशोऽध्यायः
दैवासुरसम्पद्विभागयोगः
श्री भगवानुवाच
अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।।१।।
शब्दार्थ : अभयम्-अभय, सत्त्वसंशुद्धिः- हृदय की शुचिता, ज्ञानयोग- व्यवस्थितिः- ज्ञान और योग में दृढ़ता, दानम्-दान, दमः - इन्द्रियों का संयम, च-और, यज्ञः यज्ञ, च-और, स्वाध्यायः-शास्त्रों का अध्ययन, तपः-तपस्या, आर्जवम् -सरलता ।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : अभय (भय का अभाव), हृदय की निर्मलता, ज्ञान और योग में निरन्तर दृढ़ स्थिति, दान, इन्द्रिय दमन, यज्ञ, शास्त्राध्ययन (वेदों का पठन-पाठन), तपश्चर्या और सरलता,
व्याख्या : राक्षस, असुर और देव इन तीन प्रकार के चेतन प्राणियों की प्रकृति का वर्णन भगवान् ने अध्याय 'नवम' श्लोक १२,१३ में किया है। अब इस अध्याय में विस्तार से यही वर्णन किया जा रहा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्लोक में देवता, दैवी-मनुष्य और असुरों के मध्य में स्पष्ट रूप से भेद बताया है। दैवी प्रकृति अथवा देवताओं जैसा स्वभाव मोक्ष का साधन है। आसुरी प्रकृति और राक्षसी वृत्ति बन्धन के कारण हैं। आत्म-ज्ञान-प्राप्ति में यह बाधक है। दिव्य प्रकृति को स्वीकार करना और इसी का विकास करना चाहिए। आसरी और राक्षसी वृत्ति का त्याग करना चाहिए। ये सभी गुण मनुष्यों में होते हैं। सात्त्विक मनुष्य दैवी गुणों से सम्पन्न होते हैं। मनुष्यों में भी असुर और राक्षस होते हैं जो राक्षसी गुणों से युक्त होते हैं और अत्यन्त तामसिक वृत्ति वाले होते हैं। सामान्य मानव में तीनों गुण मिश्रित रूप से होते हैं। तमस् और रजस् की ओर ले जाने वाले हैं। होता है। तमस् और रजस् बन्धन के कारण हैं। सत्त्व मोक्ष में सहायक हरिखम होत अनुशासित करो और सत्त्व का विकास करो। यह योग की नींव है। यह प्रथम सिद्धि साधन है। सत्व का विकास कर के तुम आध्यात्मिक सोपान पद्ध का एक सोपान और ऊपर चढ़ जाते हो। मन सात्विक होगा तो मन में शान्ति रहेगी। मन सौम्य हो, प्रसन्न हो तो दिव्य ज्योति का अवतरण होता है ।।
सात्विक मनुष्य इन्द्रिय-दमन करता है, निःस्वार्थ सेवा करता है, जप का अभ्यास, प्राणायाम, एकाग्रता, ध्यान, आत्म विश्लेषण और परिप्रश्न "मैं कौन हूँ", इन का अभ्यास करता है। विषय वासनायें उसे आकृष्ट नहीं करतीं। वह नम्र, उदार, दयालु, सहनशील, क्षमाशील और पवित्र होता है। अपने क्षुद्र व्यक्तित्व को वह नष्ट कर देता है। राजसिक मनुष्य अभिमानी होता है। वह असहिष्णु, अहंभाव से युक्त, स्वार्थी, कामी, क्रोधी, लोभी और ईर्ष्यालु होता है। वह नाम, यश और आत्मोत्कर्ष हेतु ही कार्य करता है। वह अपने क्षुद्र व्यक्तित्व का विकास करता है।
गुणों और कर्मों में निकट का सम्बन्ध है। कर्मों की प्रकृति गुणों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सात्त्विक मनुष्य शुभ कर्म करेगा। राजसिक और तामसिक मनुष्य अशुभ कर्म में प्रवृत्त होंगे। गुण ही मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ब्रह्म अथवा आत्मा कर्म से परे है। वह मौन साक्षी है।
प्रथम तीन श्लोकों में भगवान् दैवी मनुष्य के गुणों का उपदेश देते हैं, जो मोक्ष पथ गामी है। इसके पश्चात् वे आसुरी मनुष्य के गुणों का वर्णन करते हैं। दैवी और आसुरी प्रकृति के मध्य भेद निरूपण इस अध्याय का सार है। गुण और अवगुण सापेक्ष (relative) पद हैं, अन्योन्य संबद्ध पद हैं। एक काल का गुण दूसरे काल में अवगुण हो जाता है। अलौकिकता की दृष्टि से गुण और अवगुण का अस्तित्व ही नहीं है।
बुराई होती क्यों है, इसका अस्तित्व कहाँ से है? ये अतिप्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आत्म-ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। अनावश्यक रूप से ही लोग इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपनी बुद्धियों को (मन-मस्तिष्क को) संपीड़ित करते हैं। यह एक गम्भीर समस्या है, भूल है।
दैवी सम्पत् (दैवी सम्पदा अथवा दिव्य गुणों का ऐश्वर्य) आत्म-ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। अभय, हृदय की शुद्धि, इन्द्रिय दमन आदि सात्त्विक गुण हैं और दैवी सम्पदा हैं। वे साधक को निर्विकल्प समाधि में पहुँचाने में समर्थ हैं जो चेतना की सर्वोच्च अवस्था है और जहाँ द्रष्टा और दृश्य का सायुज्य भाव हो जाता है, ध्याता और ध्यान एक हो जाते हैं। दैवी गुण आत्मा के सर्वोच्च आनन्द की वृद्धि कराने में शक्य हैं।
दैवी गुणों में अभय होना सर्वोपरि है। अविद्या का प्रभाव (कार्य रूप) भय है। शरीर के साथ तादात्म्यता भय का कारण है। शरीर, स्त्री, बच्चे, गृह, सम्पदा आदि भय के कारण हैं। आत्म ज्ञानी सर्वथा भय मुक्त होता है।
"जहाँ से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लौट आती है उस ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला भयभीत नहीं होता।" (तैत्तिरीयोपनिषद् २.९.१)
अभय-शास्त्र के नियमों का बिना शंका किये भक्तिपूर्वक पालन करना अभय है। "मैंने सर्वस्व त्याग कर दिया है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, अब मैं कैसे रह सकता हूँ?" - इस प्रकार के भय से मुक्ति अभय की अवस्था है। संन्यास दीक्षा के समय संन्यासी संकल्प लेता है कि वह किसी प्राणी में भय नहीं उत्पन्न करेगा। अभय-दान के इस संकल्प का मनसा-वाचा-कर्मणा पालन करते हुए वह समस्त प्राणियों को अभयदान देता है। यही 'अभयम्' है। आत्मा की अमृतमयी-आनन्दमयी प्रकृति का निरन्तर चिन्तन-मनन करने से अभय प्राप्त होता है। यदि तुम ईमानदारी और सत्य पथ का अनुसरण करते हो, निःशंक हो कर शास्त्रों के विधि-विधानों का पालन करते हो, सदाचार का जीवन व्यतीत करते हो, सदा ईश्वर का स्मरण करते रहते हो तो निश्चित रूप से तुम भय से मुक्त हो जाओगे। जब मनुष्य सर्वत्र आत्म तत्त्व के दर्शन करता है, उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, जब उसमें एकत्व भाव का उदय होता है तब वह कैसे किसी से भयभीत हो सकता है और भय का भाव ही उसमें किस प्रकार से आ सकता है? मोक्ष प्राप्त करना है तो प्रथम अभय दान देने और स्वयं भयमुक्त होने का यत्न करो। मुक्त संन्यासी की प्रमुख विशेषता "अभयम्" है। किसी भी साधक की आध्यात्मिक प्रगति का यह यथार्थ मापदंड है। प्रकाश प्राप्त ज्ञानी का यह प्रधान गुण है। इसी कारण से दिव्य गुणों में यह प्रथम स्थान पर है। केवल मुक्त संन्यासी ही पूर्णतया निर्भय हो सकता है।
सात्त्विक शुभ वासना दैवी सम्पत् है। यह विवेक, वैराग्य, मनोनिग्रह और इन्द्रिय निग्रह का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है जो आत्म-ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। राग-द्वेष की धाराओं में कार्य करने को प्रेरित करने वाली, शास्त्र-निषिद्ध कर्मों को करने में उत्साहित करने वाली और आपत्तिजनक प्रभाव प्रदान करने वाली राजसिक और तामसिक वासनायें आसुरी प्रकृति की हैं।
आसुरी प्रकृति में विषय-भोगों की लालसा बनी रहती है जबकि राक्षसी प्रकृति में द्वेष भाव की प्रधानता रहती है और राक्षस अनेक प्रकार से दूसरों को कष्ट और हानि पहुँचाने का प्रयास करता है।
शुभ वासनायें मोक्ष प्रद हैं। अशुभ वासनायें बन्धन में डालती हैं। शुभ वासनाओं का विकास करना चाहिए। अशुभ वासनाओं को दूर करना चाहिए। शुभ वासनाओं को अंकुरित करने और अशुभ वासनाओं का निराकरण करने हेतु इन दोनों प्रकार की वासनाओं का ज्ञान, इनकी मूल प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। षोडश अध्याय में इन दो वासनाओं का विस्तृत वर्णन है।
सत्त्वशुद्धिः - अन्तःकरण की शुद्धि, हृदय में हर प्रकार से निर्मलता, मन की पवित्रता आदि, लोगों के साथ व्यवहार में धोखा, दम्भ आदि का त्याग और पूर्ण सत्य भाव (ईमानदारी) और एकता के भाव में रहने से सत्त्वसंशुद्धि होती है।
जब चित्त अमृत रूप आत्मा में निरन्तर स्थिरतापूर्वक अवस्थित रहने लगे तो इसे शुद्धि की अवस्था समझनी चाहिए। शुद्ध मन ही आत्म-ज्ञान कर सकता है। शास्त्र-श्रवण से जब सन्देह-निवारण हो जाते हैं, असम्भावना (आत्मा की सत्ता में सम्भावना के अभाव का विचार) से मनुष्य मुक्त हो जाता है, तब सत्त्वसंशुद्धि होती है। बिना भक्तिभाव के मन की शुद्धि सम्भव नहीं है। अतः इन सात्विक गुणों में भक्तिभाव को भी सम्मिलित किया जाता है।
ज्ञान-शास्त्रोपदेश अथवा गुरु के उपदेश के अनुरूप आत्मा की प्रकृति को समझना, उपनिषद् के महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि' पर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार ही ज्ञान है। जीवात्मा का परमात्मा के साथ सायुज्य योग है। आत्म संयम अथवा इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा अनन्यमनस्क भाव से ध्यान द्वारा अपरोक्षानुभूति (प्रत्यक्ष ज्ञान) योग है।
शास्त्र और गुरु से प्राप्त ज्ञान का अन्तर्चक्षु के द्वारा प्रत्यक्षीकरण कर के साधक संज्ञान प्राप्त करता है। साधक को अपरोक्षानुभूति होती है। वह परब्रह्म के साथ एक हो जाता है। शास्त्रों से वह परोक्ष ज्ञान अथवा मात्र, ब्रह्म का सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करता है। योग के अभ्यास से अब वह अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। सुप्त वासनाओं और मन के विनाश हेतु अपेक्षित प्रयास भी योग है।
ज्ञानयोगव्यवस्थितिः - भौतिकवाद में लिप्त मनुष्यों की मानसिकता से पृथक् ज्ञानयोग से प्राप्त जीवन्मुक्त की अवस्था ज्ञानयोगव्यवस्थिति है।
निर्भयता, पवित्रता तथा ज्ञान और योग में स्थिरता-ये तीन गुण सात्त्विक लक्षणों से युक्त हैं जिनकी व्याख्या श्लोक १ से ३ में दी गई है। ज्ञान योग ही इन गुणों से युक्त होता है। अन्य गुण ज्ञान योगियों, कर्मयोगियों, राजयोगियों और भक्तों में समान होते हैं। सात्त्विक गुणों के अभाव में किसी भी प्रकार का योग असम्भव है। एक भी गुण का यदि तुम विकास करोगे तो तुम्हारे भीतर अन्य गुण स्वतः प्रवेश करने लगेंगे। मनुष्य के आन्तरिक नैतिक निर्माण की आधारशिला निर्भयता है।
स्वाध्याय और तपस् क्रियायोग के अङ्ग हैं। ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय का रूप है। दान और यज्ञ कर्मयोग के आत्मक (अङ्ग) हैं। यज्ञ, दान और आत्म-नियंत्रण गृहस्थियों के लिए दैवी सम्पदा हैं। अध्याय XVI के श्लोक एक से तीन में वर्णित वे गुण, योग-विशेष में अभ्यास रत और उस पथ पर आरूढ़ साधक के लिए दैवी सम्पदा से युक्त हैं।
दान-भिक्षा देना, भोजन, वस्त्र आदि बांटना अपनी सामर्थ्य और साधन के अनुसार ।
दानी व्यक्ति अचिरेण दीन-दुखियों की सहायता करता है। दान तीन प्रकार का है सात्त्विक, राजसिक और तामसिक (देखो अध्याय XVII * 0.2, 21, 22 ) यह स्वर्ग के द्वार खोलने वाली प्रक्रिया है। मुक्ति के समीप ले जाने वाला कार्य है। फल देने वाले वृक्ष की भाँति बिना किसी भेद भाव के हर्षित हृदय से अकिंचन को दान दो ।
दम-आत्म संयम, इन्द्रिय-निग्रह। अन्तःकरण अथवा मन के नियन्त्रण पर निरूपण अगले श्लोक में होगा।
आत्म संयम के अभ्यास से इन्द्रियों का उनके विषयों से सम्बन्ध छूटता है। इन्द्रियाँ विषयों से पृथक् हो जायेंगी और साधक इन्द्रियों के द्वारों से विषयों की वेगपूर्ण आँधी को प्रवेश नहीं करने देगा। अब वह दृढ़तापूर्वक इन्द्रियों को संयत रखेगा। शरीर के दसों द्वारों में वह अनासक्ति रूपी अग्नि प्रदीप्त करेगा। कठोर संकल्प लेगा। मौन और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करेगा। आहार में सन्तुलित रहेगा। प्रत्येक कार्य में इस स्वर्णिम नियम का पालन करेगा। मन की तथा इन्द्रियों की बहिर्मुखी वृत्तियों को वश में रखेगा। मन और इन्द्रियों को अपने मूल स्रोत की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित करेगा। शस्त्र से जैसे शत्रु को काट दिया जाता है वैसे आत्म संयम से विषयोन्मुखी वृत्तियों का संहार किया जाता है। इन्द्रियों के दसों द्वारों में आन्तरिक उत्तेजनाओं, तृष्णाओं, वासनाओं को, परित्याग की, वैराग्य की अग्नि में भस्मीभूत कर देना चाहिए। गृहस्थी पूर्ण रूप से ऐसा संयम नहीं कर सकता किन्तु नियमित और अनुशासित जीवन ही उसके लिए आत्म संयम है। सहिष्णुता, स्थिरता, सत्य, अहिंसा और क्षमा आत्म संयम के अभ्यास में निहित हैं।
यज्ञ-वेद विहित अग्निहोत्रादि, देव पूजा, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ जो स्मृति शास्त्रों में विहित हैं- ये सब क्रियायें यज्ञ के अङ्ग हैं।
स्वाध्याय-अदृष्ट लाभ के लिए वेदों का अध्ययन करना ।
तपस् - शरीर का संयम तथा अन्य प्रकार के तप । यथार्थ तपस आत्म तत्त्व पर ध्यान एकाग्र करना है। यह आत्मा को स्थूल शरीर और अन्य चार कोषों से पृथक् करने के पश्चात् ब्रह्म सायुज्य करने की प्रक्रिया है। यह मन को अन्तर्मुखी करने की प्रक्रिया है। अध्याय XVII के श्लोक १४ से १६ में व्याचक्षित तीन प्रकार की तपश्चर्या इसी तप का अङ्ग है।
आर्जवम् -सरलता । ज्ञान प्राप्ति के लिए यह गुण अत्यन्त हितकर है। साधक को सदा निष्कपट, सत्यवादी और स्पष्ट-सरल होना चाहिए। आर्जवता उसकी निरन्तर बनी रहने वाली वृत्ति होनी चाहिए। एक न्यायप्रिय और सत्य पर आरूढ़ व्यक्ति ही सरल हो सकता है। लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वह सबका प्रिय होता है। वह समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। वह कभी सत्य को छिपाता नहीं है।
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ।।२ ।।
शब्दार्थ : अहिंसा-किसी को कष्ट न पहुँचाना, सत्यम् -सत्य (यथार्थ वचन), अक्रोधः क्रोध न होना, त्यागः-त्याग, शान्तिः-शान्ति, अपैशुनम् दोष दृष्टि का अभाव, दया-दया, भूतेषु प्राणियों में, अलोलुप्त्वम् - लोभ रहित होना, मार्दवम् -मृदुता (अक्रूरता), ही:-लज्जा, अचापलम् - स्थिरता ।
अनुवाद : अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, दोष दृष्टि का अभाव, प्राणियों के प्रति दया का भाव, अलोभ, मृदुलता, लज्जा, स्थिरता,
व्याख्या : अहिंसा-मन, वचन, कर्म से किसी को हानि न पहुँचाना। जीवित प्राणधारियों के प्रति अहिंसा भाव रखने से रजस् की शक्तियाँ अवरुद्ध होती हैं। अहिंसा भौतिक, शाब्दिक और मानसिक तीन प्रकार की होती है।
सत्यम् - असत्य और अप्रिय वचन बोले बिना किसी वस्तु का यथार्थ वर्णन सत्य है। सत्य में आत्म-संयम, ईर्ष्या का अभाव, क्षमा, सहिष्णुता, धैर्य और दया आदि गुण निहित हैं।
अक्रोधः दूसरों के द्वारा अपमानित होने पर, गाली दी जाने पर अथवा ताड़ना मिलने पर क्रोध न करना अक्रोध है।
त्यागः-त्याग । कर्मफल, अहंकार और वासनाओं का त्याग । दान भी त्याग है, इसका वर्णन पूर्व श्लोक में आ चुका है।
शान्तिः- संकल्परहित अन्तःकरण ।
अपैशुनम् -क्षुद्रता का अभाव।
दया-दुखियों पर करुणा भाव रखना। दयालु व्यक्ति का हृदय कोमल होता है। वह संसार के कल्याण के लिए जीता है। अन्य प्राणियों के साथ ऐक्य भाव दया है।
अलोलुप्त्वम् लोभ न करना। लोभ न हो तो इन्द्रियाँ, अपने-अपने विषयों के सम्पर्क में आने पर भी उत्तेजित अथवा प्रभावित नहीं होतीं। कूर्म के अङ्गों की भाँति इन्द्रियों का विषयों से प्रत्याहरण हो जाता है।
ह्री:-समाज और वेदों के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर लज्जा का अनुभव ही है।
अचापलम्-बिना प्रयोजन हाथ-पैर और वाणी की चेष्टा न करना और व्यर्थ की चेष्टायें न करना "अचापलम्" है। आर्जव, अहिंसा, अक्रोध आदि ब्राह्मणों के विशेष गुण हैं। ये उनके सात्त्विक गुण हैं।
और भी-
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ।।३ ।।
शब्दार्थ : तेजः-तेज, क्षमा-क्षमा, धृतिः- धैर्य, शौचम् - पवित्रता, अद्रोहः-द्वेषहीनता, नातिमानिता-अत्यन्त अभिमानी न होना, भवन्ति-होते हैं, संपदम् गुण, दैवीम् - दैवी, अभिजातस्य-जन्म लेने वाले के, भारत-हे भरतवंशी अर्जुन ।
अनुवाद : तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेषहीनता, अभिमानी न होना-ये सब गुण दैवी सम्पत् को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष में होते हैं।
व्याख्या : तेजस्-तेज, शक्ति, दीप्ति, त्वचा की आभा (चमक) । मोक्ष के लिए जिज्ञासु साधक आध्यात्मिक पथ पर साहस के साथ आरूढ़ होता है। उसकी उन्नति में कोई शिथिलता नहीं ला सकता। कोई वस्तु उसे आकर्षित नहीं कर सकती । आत्म साक्षात्कार हेतु यह सतत अटूट उत्कर्ष तेजस् है। यह तमस् की निम्नगामी प्रकृति का अतिक्रमण करता है।
क्षमा-इस गुण से युक्त मनुष्य अपमानित होने पर, अपशब्द कहे जाने पर अथवा ताड़ना दिये जाने पर भी क्रोध नहीं करता, यद्यपि उसमें प्रत्यपकार अथवा प्रतिहिंसा की शक्ति होती है, तथापि वह हिंसा अथवा अपमान से अप्रभावित रहता है।
धृति-यति अपने भीतर समस्त विपदाओं को विलीन कर लेता है।
अत्यन्त पीड़ादायक परीक्षा की घड़ी में भी स्थिर बना रहता है - यह एक विशेष सात्त्विक वृत्ति अथवा मनोदशा है जो शरीर तथा इन्द्रियों की शिथिलता में उनका अवसाद अथवा थकावट दूर करती है। इस दिव्य गुण से युक्त साधक कठिन से कठिन परीक्षण-काल में भी, कठिनाइयों में भी उद्विग्न नहीं होता । शरीर और इन्द्रियाँ जब शिथिल हों तो धृति (वृत्ति) उस समय उत्तेजक शर्बत की काम करती है।
शौचम् - पवित्रता। यह दो प्रकार की है-बाह्य शुद्धि और
भाँति एक 'टॉनिक' का अन्तः शुद्धि । बाह्य शुद्धि के लिए जल और मिट्टी साधन हैं। अन्तःकरण माया से मुक्त हो जाए तो आन्तरिक शुद्धि होती है। माया क्या है? धोखा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या-द्वेष, दम्भ आदि ये दुर्गुण माया के वश से हैं इनका निराकरण ब्रह्मचर्य, क्षमा, मित्रता, दान, नम्रता, सौम्यता, प्रेम, दया आदि गुणों के विकास से होता है। ये सद्गुण आ जायें तो अन्तःकरण स्वतः शुद्ध हो जाता है। बाह्य शुद्धि की अपेक्षा आन्तरिक शुद्धि अधिक महत्त्वपूर्ण है।
अद्रोह-घृणा के भाव का अभाव, दूसरों को चोट पहुँचाने के भाव का अभाव ।
अतिमानिता-अत्यन्त अभिमान । अभिमानी मनुष्य स्वयं को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठतर समझता है और मान की आकाचा रखता है। नातिमानिता, इस गुण के विपरीत है। तेजस्, क्षमा और धृति क्षत्रियों के विशेष गुण हैं। ये क्षत्रियों के सात्त्विक गुण हैं। शौच और अद्रोह वैश्यों के विशेष धर्म हैं। ये गुण वैश्यों अर्थात् व्यापारियों के वर्ग के लिए सात्त्विक गुण हैं। नातिमानिता अर्थात् अभिमान का अभाव शूद्र जाति का विशेष गुण है और यही उनका सात्त्विक गुण है।
दैवी सम्पत् छब्बीस गुणों से युक्त है। यह परमात्मा की विरल देन है। यह ऐसी अक्षय्य सम्पदा है जिसे डाकू लूट नहीं सकते। ये सम्पदा साधक को अविनाशी, अनघ ब्राह्निक पद प्राप्ति में सहायक है। यह मोक्ष प्राप्ति का सरल साधन है।
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ।।४ ।।
शब्दार्थ : दम्भः- धर्मध्वजिन् (कपटी), दर्पः- गर्व, अभिमानः अहंकार, व-और, क्रोधः क्रोध, पारुष्यम् -कठोरता, एव-ही, च-और, अज्ञानम्-अज्ञान, चऔर, अभिजातस्य-उत्पन्न हुए (मनुष्य के), पार्थ- हे पार्थ, सम्पदम् लक्षण, आसुरीम् आसुरी ।
अनुवाद : दम्भ, कपट, गर्व, अभिमान (आत्म प्रवंचना), क्रोध, कठोरता और अज्ञान-ये सब लक्षण, हे पार्थ, आसुरी सम्पदा को ले कर उत्पन्न हुए मनुष्य के हैं।
व्याख्या : दम्भ-कपट । मनुष्य जो नहीं है वही होने का नाटक करना, धार्मिक नहीं है किन्तु फिर भी धार्मिक और पवित्र (धर्मध्वजी) बनने का दिखावा करना। इसमें आत्मश्लाघा भी निहित है। धार्मिक कपट तो निकृष्ट कोटि का कपट है। दम्भ, धोखे और असत्य का मिश्रित रूप है। अहंकारवश आत्म श्लाघा करने वाले पाप के भागी होंगे।
दर्प-गर्व। विद्या, धन, मान आदि का गर्व। दर्पयुक्त व्यक्ति अपने सहचरों को प्रसन्न नहीं देख सकता। मित्रों की सुख-समृद्धि और विद्या-अर्जन में वह उनके सौभाग्य पर क्रोधित होता है।
पारुष्यम् - वाणी में कठोरता। अन्धे को कमलनयन वाला कहना, कुरूप को सुन्दर कहना, हीन जाति वाले को उत्तम जाति वाला कहना आदि ये आक्षेप अत्यन्त स्वार्थ भाव में किये जाते हैं।
अज्ञानम् अपने कर्तव्य के प्रति गलत धारणा । अज्ञानी व्यक्ति किंकर्तव्यविमूढ़ होता है। उसमें विवेक नहीं होता। जिस प्रकार एक शिशु कोई भी वस्तु उठा कर मुख में डाल लेता है, स्वच्छ और दूषित का ध्यान नहीं करता, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति विवेक-शून्य होने के कारण सत्य-असत्य, शुभ-अशुभ, गुण-अवगुण का विचार नहीं करता। वह विनाश पथ पर आरूद रहता है। मोक्ष पथ का तो उसे ज्ञान ही नहीं होता । भौतिक अस्तित्व के सागर में ही वह डूब जाता है।
ये छः आसुरी गुण हैं। ये बुरे गुण आसुरी सम्पदा के अन्तर्गत माने जाते हैं। मोक्ष पथ के ये प्रतिबन्धक हैं।
अर्जुन को 'पार्थ' कह कर, सम्बोधन कर के भगवान् यह संकेत दे रहे हैं कि अर्जुन में ये आसुरी गुण नहीं हैं क्योंकि वह पृथा के उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है।
आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य विश्वसनीय नहीं होते । वे प्रत्येक सिद्धान्त पर तर्क करेंगे। वे परमात्मा की सत्ता को नकारते हैं। वे संसार चक्र को नहीं मानते और वेद-विरुद्ध, नैतिक गुणों के विरुद्ध चलते हैं। विषयों का सङ्ग ही उनका ध्येय है। वे लोगों को लूटते हैं, पर-स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं। क्रूरता से लोगों की हिंसा करते हैं। वे पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास नहीं रखते । आत्म संयम, सदाचार और शुचिता उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते ।
असुर वे मनुष्य हैं जिन्होंने आक्रमण किये और अभी भी स्वर्ग में देवताओं के साथ युद्ध कर रहे हैं। आसुरी वृत्ति अथवा दुर्गुणों से युक्त मनुष्य ही असुर अथवा राक्षस हैं। इस कलियुग में वे बहुलता में हैं। कंस एक असुर था। हिरण्यकश्यपु एक असुर था।
विश्वविद्यालय से शिक्षा एवम् उपाधि प्राप्त पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी यदि इन अशुभ वासनाओं से युक्त है तो वह असुर ही है।
अलौकिक रूप से असुर और देवताओं के मध्य आन्तरिक युद्ध शुभ-अशुभ वृत्तियों के रूप में अथवा सत्त्व और रजस्-तमस् के रूप में मनुष्य में निरन्तर चलता रहता है।
दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ।।५ ।।
शब्दार्थ : दैवी-दैवी, सम्पत् -सम्पदा, विमोक्षाय-मोक्ष के लिए, निबन्धाय-बन्धन के लिए, आसुरी-आसुरी, मता-मानी गई है, मा-नहीं, शुचः-शोक करो, सम्पदम् अवस्था, दैवीम् - दिव्य (देव सम्बन्धी), अभिजातः-उत्पन्न हुए, असि-हो, पाण्डव- हे पाण्डव ।
अनुवाद : दिव्य प्रकृति मोक्ष के लिए हितकर है और आसुरी प्रकृति बन्धन में डालने वाली है। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, तुम दिव्य गुणों से युक्त हो कर जन्मे हो।
व्याख्या : सम्पत् सम्पत्ति, ऐश्वर्य की अवस्था, प्रकृति, गुण। मोक्ष-संसार चक्र, जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्ति। दिव्य प्रकृति मोक्षप्रद है और आसुरी बन्धन के लिए है।
अर्जुन पूर्वतः ही शोकग्रस्त और अवसाद की स्थिति में था, अतः भगवान् कृष्ण उसे सान्त्वना देते हुए कहते हैं कि वह आसुरी गुणों के वर्णन से दुःख का अनुभव न करे और मोह में न फंसे क्योंकि वह तो मोक्षप्रद सात्त्विक वृत्तियों को ले कर उत्पन्न हुआ है। भगवान् के इन शब्दों को श्रवण कर के अर्जुन ने सोचा होगा- "मैं दिव्य गुणों से युक्त हूँ अथवा आसुरी प्रकृति का हूँ?" भगवान् ने अर्जुन का सन्देह निवारण करने के लिए कहा- "हे अर्जुन, शोक मत करो। तुम दैवी सम्पदा से युक्त हो कर अवतरित हुए हो। तुम सौभाग्यशाली हो । तुम मोक्ष का आनन्द प्राप्त करोगे।"
"हे अर्जुन, ऐसा मत सोचो कि युद्ध में संलग्न हो कर, हिंसा कर के तुम असुर बन जाओगे। इस पर शोक मत करो। इस धर्मयुद्ध को लड़ कर तुम धर्म राज्य की स्थापना करोगे।"
द्वौ भूतसर्गों लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च ।
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ।। ६ ।।
शब्दार्थ : द्वौ दो, भूतसर्गों-जीवों की सृष्टियाँ, लोके-लोक में, अस्मिन् - इस (में), दैवः - दिव्य, आसुरः- आसुरी, एव-ही, च-और, दैवः-दिव्य (दैवी), विस्तरशः - विस्तार से, प्रोक्तः-कहा गया, आसुरम् - आसुरी, पार्थ-हे पार्थ, मे-मुझे, शृणु सुनो।
अनुवाद : हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के सृजित प्राणी हैं-दैवी और आसुरी। दैवी का वर्णन विस्तार से हो चुका है अब तुम आसुरी गुणों के विषय में मुझ से श्रवण करो।
व्याख्या: दैवी और पैशाचिक दो प्रकार के सृजित प्राणी अपनी-अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप कार्यरत रहते हैं।
बृहदारण्यकोपनिषद् में भी वर्णन आता है-
“निश्चित रूप से सृष्टिकर्ता के जीवों के दो वर्ग हैं-देव और असुर ।" (१.३१)
भूतसगौं-जीवों की सृष्टियाँ। प्राणियों की जातियाँ। सृष्टि का अभिप्राय यहाँ सृष्टि में सृजित जीवों से है। दैवी और आसुरी प्रकृति वाले दो प्रकार से सृजित मनुष्य ही दो प्रकार की सृष्टियाँ नाम से अभिहित हैं। प्रत्येक मनुष्य, इस संसार में एक अथवा अन्य दो, दैवी और आसुरी वर्ग के अन्तर्गत आता है।
भगवान् कृष्ण अर्जुन से कहते हैं-"अब मैं तुम्हें आसुरी गुणों से युक्त व्यक्तियों के लक्षण बताऊँगा। यदि तुम्हें आसुरी गुणों का ज्ञान हो जायेगा तो तुम उनसे दूर रहोगे।" इस अध्याय के अन्त तक आसुरी वृत्ति का वर्णन विस्तारपूर्वक किया जाता है।
अध्याय IX श्लोक 9,11,12 में आसुरी वृत्ति का वर्णन है। किन्तु वर्णन अपूर्ण होने के कारण इस अध्याय में इसे विस्तार से बताया जा रहा है।
श्री भगवान् ने दैवी प्रकृति का विस्तृत वर्णन पूर्वाध्यायों में किया है स्थितप्रज्ञ की अवस्था अध्याय II में, भागवत पुरुष की अवस्था अध्याय XII में और त्रिगुणातीत की अवस्था का वर्णन XIV तथा इसी अध्याय के प्रथम तीन श्लोकों में किया गया है।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ।।७ ।।
शब्दार्थ : प्रवृत्तिम् -कर्तव्य कर्म को, च-और, निवृत्तिम्-अकर्म को, च और, जनाः मनुष्य, न-नहीं, विदुः -जानते, आसुराः आसुरी गुण वाले, न-नहीं, शौचम् - पवित्रता, न-नहीं, अपि-भी, च-और, आचारः- आचरण, न-नहीं, सत्यम् -सत्य, तेषु उनमें, विद्यते - है।
अनुवाद : आसुरी व्यक्ति ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए । उनमें न तो पवित्रता होती है न सदाचार और न ही सत्य भाषण ।
व्याख्या : आसुरी प्रकृति वाले लोग कर्म और अकर्म (कर्महीनता) की प्रकृति को नहीं जानते । शरीर के अतिरिक्त आत्मा का विचार, निष्क्रिय रह कर केवल गुणों की लीला को देखना उनकी बुद्धि से परे है। वे दूसरों की रुचि का सर्वथा ध्यान नहीं रख सकते। वे अपने शरीर अथवा इन्द्रिय सन्तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। वे लोभी, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। अतः न तो उनका चरित्र अच्छा होता है और न व्यवहार। वे असत्यभाषी, अन्यायी और अपवित्र होते हैं। वे नहीं जानते कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और बुराई से बचने के लिए क्या करना चाहिए।
आसुरी प्रकृति के व्यक्ति तो मानो अविद्या रूपी पंक में डूबे हुए हैं। निषिद्ध कर्म कौन-कौन से हैं और शास्त्र-विहित कर्म कौन से हैं, इससे वे सर्वथा अनभिज्ञ रहते हैं। पवित्रता की धारणा तो उनमें कदापि नहीं होती। उनके कर्म कुटिल होते हैं। न तो वे यथार्थ प्रवृत्ति का और न ही यथार्थ निवृत्ति का ज्ञान रखते हैं। धर्म-अधर्म, शास्त्रोपदेश, निर्देश वे नहीं जानते। वे कभी प्रिय नहीं बोलेंगे। वे मिथ्याभाषी और दम्भी होते हैं।
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ।।८ ।।
शब्दार्थ : असत्यम् - मिथ्या, अप्रतिष्ठम् - आधार रहित, ते-वे, जगत् संसार, आहुः-कहते हैं, अनीश्वरम् - बिना ईश्वर के, अपरस्परसम्भूतम् - परस्पर संयोग से उत्पन्न, किम् -क्या, अन्यत्-अन्य, कामहैतुकम् -काम के कारण ।
अनुवाद : वे कहते हैं- "यह जगत् असत्य है, प्रतिष्ठा रहित है अर्थात् इसका कोई नैतिक आधार नहीं है, इसका कोई स्वामी नहीं है, यह काम से प्रेरित स्त्री-पुरुष के परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ है और काम ही इसका कारण है अन्य कुछ नहीं।
व्याख्या : वे विश्व को बिना किसी आश्रय का अथवा बिना किसी नित्य मूल सत्ता का मानते हैं।
यह चार्वाक और अन्य भौतिकवादी नास्तिक (अनीश्वरवादी) लोगों की विचारधारा है। वे ब्रह्म की सत्ता को नकारते हैं जो इस जग का आधार है। वे ईश्वर की सत्ता का भी निषेध करते हैं। वे कहते हैं- "हम मिथ्या हैं इसलिए जगत् भी मिथ्या है। सत्य की घोषणा करने वाले शास्त्र भी मिथ्या हैं। अधिक क्या? काम ही इस जगत् का कारण हो सकता है। परस्पर संयोग ही एकमात्र जीवों की उत्पत्ति का कारण है। कर्म का सिद्धान्त कुछ नहीं है। काम से प्रेरित हो कर स्त्री-पुरुष के सम्भोग के कारण ही इस संसार का उद्भव हुआ है। अधर्म और धर्म कुछ नहीं है। धर्माधर्म के अनुसार कर्मों के फल प्रदान करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। कामेच्छा ही इसका एकमात्र कारण है। यह संसार बस एक घटना है।" उनमें अन्तर्निरीक्षण की प्रतिभा नहीं होती। वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से अनभिज्ञ होते हैं।
अपरस्पर सम्भूतम् सम्भोग । इस का अभिप्राय अणुओं का संयोग भी हो सकता है। वैशेषिक मतानुसार संसार अणुओं के संयोग से सृजित है।
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।।९ ।।
शब्दार्थ : एताम् -इस, दृष्टिम् - दृष्टि (विचारधारा) को, अवष्टभ्य- स्वीकार कर के, नष्टात्मानः नष्ट (अज्ञानी) आत्मायें, अल्पबुद्धयः - अल्प बुद्धि वाले, प्रभवन्ति-उत्पन्न होते हैं, उग्रकर्माणः क्रूर कर्मी, क्षयाय-नाश करने के लिए, जगतः-जगत् का, अहिताः - शत्रु ।
अनुवाद : इस विचारधारा का अवलम्बन लेकर ये अल्पबुद्धि, नष्टात्मा और क्रूरकर्मा लोग संसार के विनाश के लिए शत्रु रूप में उत्पन्न होते हैं।
व्याख्या : वे दूसरों को लूटते हैं। दूसरों का विनाश कर के उनकी धन-सम्पदा पर अधिकार करते हैं। अपने बुरे कर्मों का गर्व करते हैं।
नष्टात्मानः नष्ट आत्मायें जिन्होंने आत्म साक्षात्कार के सब अवसर खो दिये और उच्चतर लोकों में भी प्रवेश पाना उनके लिए सर्वथा असम्भव है।
अल्पबुद्धयः-वे अल्पबुद्धि होते हैं क्योंकि अशुद्धियों से पूर्ण इस शरीर को ही वे आत्मा मानते हैं, परमात्मा का उन्हें कोई ज्ञान नहीं और उनकी वृत्तियाँ विषय-वासनाओं में ही अटकी रहती हैं। खाना-पीना-सोना उनके जीवन का ध्येय बन जाता है।
उग्रकर्माणः - क्रूरकर्मा। वे हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। धन प्राप्ति के लिए हिंसा करने में भी हिचकिचाते नहीं। श्री और स्त्री को प्राप्त करने के लिए वे कोई भी घृणित कार्य कर सकते हैं। भ्रम जाल फैला कर वे संसार की शान्ति और समन्वय को नष्ट करते हैं।
जगतः अहिताः संसार के शत्रु । जगत् का अर्थ यहाँ लोगों से है जो संसार में रहते हैं।
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।
मोहाद्गृहीत्वासङ्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ।।१०।।
शब्दार्थ : कामम् - इच्छा का, आश्रित्य-शरण लेकर, दुष्पूरम् -कभी सन्तुष्ट न होने वाली, दम्भमानमदान्विताः- दम्भ (गर्व), मान (झूठी प्रतिष्ठा), और मद से युक्त हुए, मोहात्-मोह वश, गृहीत्वा-ग्रहण कर के, असद्द्याहान् असत्य सिद्धान्तों के, प्रवर्तन्ते-व्यवहार करते हैं, अशुचिव्रताः- अशुद्धाचारी, अपवित्र संकल्प वाले ।
अनुवाद : कभी पूर्ण न होने वाले काम का आश्रय लेकर, दम्भ, मान और अहंकार से युक्त, भ्रम वश अशुभ विचारों को ग्रहण कर के वे अपवित्र संकल्पों से व्यवहार करते हैं।
व्याख्या : ये अज्ञानी दुरात्मन् मनुष्य क्रूर पाप कर्म करते हैं। उनकी बुद्धि दर्प, छल-कपट और अभिमान से परिपूर्ण होती है। वे अशुभ संकल्प वाले और तर्करहित विचारों से युक्त होते हैं। वे अपने अन्तःकरण में कभी सन्तोष को प्राप्त न होने वाली इच्छाओं को सींचते हैं। वानर को मदिरा पान कराई जाये तो और अधिक उन्मादक हो जाता है। ऐसे ही वे जैसे-जैसे वयोवृद्ध होते हैं वैसे ही और अधिक कामी और अभिमानी होते जाते हैं। वे अपने परिवेश के लोगों को नष्ट करते हैं और उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। उन्हें अपने कर्मों पर अभिमान होता है। दूसरों को वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें अपने शरीरों से अत्यन्त आसक्ति होती है। अपने शरीर की तो वे पूजा ही करते हैं। उनका मोह असीम होता है। वे मूर्ख और हठी होते हैं अतः उनका कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता।
आशायें-इच्छायें अग्नि की भाँति कभी सन्तुष्ट नहीं होतीं। मनोरञ्जन से इच्छाओं की सन्तुष्टि नहीं होती। अधिक सुख भोगते हो, अधिक ही इच्छायें जाग्रत होती हैं। एक विषय का सुख भोगने के उपरान्त सदा-सदा के लिए सुख-भोग की इच्छा बनी रहती है। विषयों के संरक्षण हेतु तुम हर प्रकार का साधन करते हो ।
धर्मावलम्बी न होते हुए भी मनुष्य धार्मिक होने का दिखावा करता है। यह दम्भ है। सम्मान के योग्य न होने पर भी वह सम्मान की आकाङ्क्षा करता है। यह मान है। यह झूठी प्रतिष्ठा है। मिथ्या अनुभाव है। उत्कृष्ट वस्तुओं से वंचित होने पर भी वह उन्हें स्वयं पर आरोपित करता है। यह मद है।
असुर अशुभ संकल्प करते हैं- "मैं अमुक देवता की आराधना अमुक मन्त्र से करूँगा और अमुक नारी पर अधिकार करूँगा । अमुक मन्त्र का जप करके अमुक व्यक्ति की हिंसा करूँगा।"
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।।११ ।।
शब्दार्थ : चिन्ताम् -चिन्ता, अपरिमेयाम् - अपार , च -और, प्रलयान्ताम् - मृत्यु पर्यन्त, उपाश्रिताः- आश्रित, कामोपभोगपरमाः- इन्द्रिय तृप्ति को परम लक्ष्य मानने वाले, एतावत् - इतना ही, इति-इस प्रकार, निश्चिताः - निश्चय करके ।
अनुवाद : मृत्यु पर्यन्त साथ रहने वाली अगणित अपार चिन्ताओं का आश्रय लेते हुए, इन्द्रिय-तृप्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए और यह विषय-भोग ही परम पुरुषार्थ है-ऐसा सोचने वाले,
व्याख्या : अपरिमित चिन्ताओं, क्लेशों और उत्सुकताओं से परिपूर्ण उनके मन अगणित इन्द्रिय विषयों की प्राप्ति और संरक्षण में लगे रहते हैं। उनका यह दृढ़ निश्चय होता है कि इन्द्रियों का सुख भोग ही मानव जीवन का आत्यन्तिक लक्ष्य है। वे विषय भोग में ही निमज्जित रहते हैं। वे इसी को ही सर्वस्व मानते हैं। विषय-भोग को वे आनन्द का परम स्रोत मानते हैं। उनके लिए आत्मा के अलौकिक शाश्वत आनन्द जैसी कोई वस्तु नहीं है। दूसरे लोक के सुख का उन्हें विश्वास ही नहीं है। इन्द्रियों की पहुँच से परे (इन्द्रियातीत) सुख, इन्द्रियों की आधीनता से मुक्त अक्षय्य आनन्द की वे कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि स्थूल और मूढ़ होती है। वे उच्चतर सूक्ष्म सत्य का ज्ञान नहीं कर सकते और न ही ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ हैं। इन्द्रिय-भोग ही उनकी सर्वोच्च प्राप्ति है।
आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ।।१२ ।।
शब्दार्थ : आशापाशशतैः- आशाओं के सैकड़ों बन्धनों से, बद्धा:-बद्ध, कामक्रोधपरायणाः क्रोध और काम के आश्रित, ईहन्ते-इच्छा करते हैं, कामभोगार्थम् -काम-भोग के निमित्त, अन्यायेन-अन्याय से, अर्थसञ्चयान् - धन का संग्रह।
अनुवाद : आशाओं के सैकड़ों पाशों से बन्धे हुए, काम-क्रोध परायण वे इन्द्रिय-भोग हेतु अवैध रूप से धन सञ्चय की कामना करते हैं।
व्याख्या : विषय भोगों के निमित्त वे हिंसा और लूटमार के कुकृत्यों में संलग्न होते हैं। धन संचय वे विषय-भोग के लिए करते हैं शुभ कर्मों में लगाने के लिए नहीं। उनमें लेशमात्र भी दया भाव नहीं होता। वे अत्याचारी होते हैं। आशाओं के शत-शत-पाशों से वे बंधे होते हैं। अपने हृदय में वे अनेक प्रकार के विषयों के भोग हेतु तृष्णाओं को आश्रय देते हैं। अनेक इच्छायें उनके मन में अंकुरित होती हैं। इच्छापूर्ति न होने पर वे हिंसक हो जाते हैं। अन्यायपूर्ण ढंग से वे धन संचित करते हैं। आशायें मनुष्य को संसार में आवृत करती हैं। इसीलिए आशा को पाश कहा गया है। उनकी तृष्णाओं का कोई अन्त नहीं होता। विशाल धन राशि एकत्र कर लेने पर भी उनकी तृष्णायें शान्त नहीं होतीं। वे तो दिन-दिन द्विगुणित होती हैं। ऐसे व्यक्ति लोभ के व्यर्थ शिकार बनते हैं।
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ।।१३ ।।
शब्दार्थ : इदम् यह, अद्य-आज, मया-मेरे द्वारा, लब्धम् - प्राप्त किया गया है, इमम् - इसको, प्राप्स्ये-प्राप्त करूँगा, मनोरथम् - इच्छा को, इदम् - यह, अस्ति-है, इदम्-यह, अपि-भी, मे-मेरा, भविष्यति - होगा, पुनः पुनः, धनम् - धन।
अनुवाद : "आज मैंने इस (द्रव्य) को प्राप्त कर लिया है, अपना अमुक मनोरथ भी पूर्ण करूँगा। यह (धन) मेरा है और भविष्य में यह धन भी मेरा हो जायेगा।”
व्याख्या : "मैं वह सब प्राप्त करने में समर्थ हो जाऊँगा जो कुछ भी संसार में है। तब मैं ऐश्वर्य का स्वामी हो जाऊँगा। इस धरा पर मेरे समान अन्य कोई न होगा।"
भविष्य में- "आगामी वर्ष में यह सम्पदा भी मेरी हो जायेगी। मैं संसार में एक समृद्ध (धनी) व्यक्ति के रूप में जाना जाऊँगा। लोग मुझे 'मेरे स्वामी' कह कर पुकारेंगे।"
ये असुर (जो इस प्रकार सोचते हैं) अपनी सम्पत्ति के कारण ही आत्मप्रवञ्चना के शिकार हो जाते हैं। अभिमान से वे फूले रहते हैं। दूसरों को वे तृणवत् व्यर्थ समझते हैं। धन का अभिमान उनके विवेक का हरण कर लेता है। वे सुख की आकाङ्क्षा करते हैं किन्तु कभी सुखी हो नहीं पाते। वे माया-जाल में फंस जाते हैं। इहलोक और परलोक में पाप और दुःख ही उनका पाणिग्रहण करते हैं।
असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ।।१४ ।।
शब्दार्थ : असौ-वह, मया-मेरे द्वारा, हतः- मारा गया, शत्रुः-शत्रु, हनिष्ये-मारूँगा, च-और, अपरान् - अन्यों को, अपि-भी, ईश्वरः ईश्वर, अहम् -मैं, अहम् -मैं, भोगी-भोगने वाला, सिद्धः-सिद्ध, अहम् -मैं, बलवान् बलशाली, सुखी-सुखी ।
अनुवाद : वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है अन्य शत्रुओं का भी संहार करूँगा। मैं ईश्वर हूँ। मैं भोगी हूँ। मैं सिद्ध हूँ, बलवान् और सुखी हूँ।
व्याख्या : मैं जो भी ईक्षण करता हूँ उस सब का ईश्वर बनूँगा। मेरी सेवा न करने वालों को मैं जीवित नहीं छोडूंगा। वस्तुतः सृष्टि का स्वामी मैं हूँ। मैं अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करूँगा। मेरे पास प्रचुर भूमि, पशुधन और सम्पत्ति है। मेरे अनेक पुत्र-पौत्र हैं। इन्द्र भी मेरा सामना नहीं कर सकता, वह मेरे सम नहीं है। मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। मैं हर प्रकार से शक्तिवान्, बलवान्, स्वस्थ और सुखी हूँ।
इस श्लोक में आसुरी प्रकृति वाले लोगों की व्यर्थ कल्पनाओं का वर्णन है।
आढ्यो ऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।। १५ ।।
शब्दार्थ : आढ्यः- धनवान्, अभिजनवान् - अच्छे कुल में उत्पन्न, अस्मि (मैं) हूँ, कः कौन, अन्यः-अन्य, अस्ति-है, सदृशः समान, मया-मुझसे, यक्ष्ये-यज्ञ करूँगा, दास्यामि-दान करूँगा, मोदिष्य-हर्ष मनाऊँगा, इति-इस प्रकार, अज्ञानविमोहिताः- अज्ञान से मोहग्रस्त ।
अनुवाद : मैं धनवान् हूँ। कुलीन परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे सदृश और कौन है? मैं यज्ञानुष्ठान करूँगा। दान करूँगा। हर्ष मनाऊँगा," इस प्रकार अज्ञान से विमोहित,
व्याख्या : "धन का देवता कुबेर धनवान् हो सकता है किन्तु मेरे तुल्य नहीं हो सकता। और तो और, भगवान् विष्णु के पास भी इतनी सम्पत्ति नहीं है जितनी मेरे पास है। मेरे कुलीन वंश और सगे सम्बन्धियों की तुलना में तो ब्रह्मा की कुलसंतति भी तुच्छ है। वे मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। सम्पूर्ण विश्व में मेरे समकक्ष कौन हो सकता है?"
अभिजनवान् सात पीढ़ियों से श्रोत्रिय आदि गुणों से सम्पन्न वंश में जन्म हो जिसका वह अभिजनवान् है। "इस विषय में मेरे समान दूसरा कोई नहीं। नाम और ख्याति उपलब्ध करने के लिए मैं यज्ञादि करूँगा। इसमें भी मेरा उपमान कोई नहीं बन सकता। मेरी स्तुति में नृत्य-गीत-संगीत करने वालों को मैं धन-दान और उपहार भेंट करूँगा। दान देने में मेरे समान कोई नहीं होगा। मैं भक्षण, मदिरापान और नारी में प्रमोद मनाऊँगा।"
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।।१६ ।।
शब्दार्थ : अनेक-अनेक, चित्तविभ्रान्ताः- (चिन्ताओं से) भ्रान्त चित्त, मोहजालसमावृताः- मोह-जाल में फंसे हुए, प्रसक्ताः- आसक्त हुए, कामभोगेषु विषय-भोगों में, पतन्ति-गिरते हैं, नरके-नरक में, अशुचौ-अशुद्ध ।
अनुवाद : मनःकल्पित वासनाओं के कारण भ्रान्त चित्त, मोह-जाल में फंसे हुए और इच्छाओं की तृप्ति के आदि बने हुए वे अपवित्र नरक में गिरते हैं।
व्याख्या: उग्र ज्वर में जिस प्रकार मनुष्य असंगत शब्दों का उच्चारण करता है उसी प्रकार ये पिशाचोपम मनुष्य अपनी इच्छाओं और इन्द्रिय-भोगो का बहुत प्रलपन करते हैं। अनेक पाप करने के उपरान्त वे वैतरणी सदृश घोर अशुद्ध नरक में गिरते हैं। मोह एक जाल है क्योंकि वह जाल की भाँति फंसाने बाला है। मछली की भाँति वे मोह जाल में फंस जाते हैं। चारों ओर से वे जाल से घिरे होते हैं। वे भ्रमित हो जाते हैं कि अब क्या करें और क्या न करें। अनेक प्रकार के कुविचारों को आश्रय दे कर वे मोहग्रस्त हो जाते हैं। उचित-अनुचित, लाभप्रद-हानिप्रद और कल्याण-अकल्याण के मध्य विवेक दृष्टि रखना वे नहीं जानते । ज्ञान का अभाव अथवा उचित-अनुचित का ज्ञान न होना ही मोह है। क्योंकि मोह एक आवरण है और बन्धन का कारण है इसकी तुलना जाल से की गई है। उपर्लिखित समस्त गुण पतन की ओर ले जाते हैं।
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ।।१७ ।।
शब्दार्थ : आत्मसंभाविताः-अपने को श्रेष्ठ मानने वालो, स्तब्धाः - विनयरहित, धनमानमदान्विताः- धन तथा झूठी प्रतिष्ठा के मद से युक्त, यजन्ते-यज्ञ करते हैं, नामयज्ञैः- नाम मात्र के लिए यज्ञ, ते-वे, दम्भेन-पाखण्ड से (धर्मध्वजीपन से), अविधिपूर्वकम् - बिना किसी विधि विधान के।
अनुवाद : स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले, विनय रहित, धन और मान के मद से युक्त, पाखण्ड से, नाम के लिए, अविधिपूर्वक यज्ञों द्वारा पूजन करते हैं।
व्याख्या : असीम अभिमान् से वे फूलते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। साधुजनों द्वारा वे आदरणीय नहीं माने जाते । अपनी महानता पर उन्हें विशेष गर्व होता है। वे सोचते हैं वे सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त हैं। वे नम्र नहीं होते। उनमें विनय और शीलता का अभाव होता है। उनके मन पूर्ण रूप से अपनी ही महानता के भाव से पूर्ण होते हैं। दूसरों को वे हेय दृष्टि से देखते हैं। वे सोचते हैं कि अन्य लोग उनसे छोटे हैं। यति, संन्यासी, वृद्ध अथवा आध्यात्मिक गुरु को वे प्रणाम नहीं करते, वे कभी अपना शीश नहीं झुकाते । धन की मदिरा से उन्मत्त वे स्तम्भ की भाँति सीधे खड़े रहते हैं। यज्ञ करने का पाखण्ड करते हैं।
न तो वे वेदी का ध्यान रखते हैं न पर्णशाला अथवा यज्ञ कुण्ड का अथवा यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली किसी उचित वस्तु का ध्यान करते हैं। शास्त्र-विहित नियमों का वे विचार नहीं करते। अपनी ख्याति बढ़ाने हेतु वे यज्ञ करते हैं। वे तो ब्रह्म का नाम भी सुन कर ध्यान नहीं देते तो भगवान् उनके अनुष्ठानों पर कैसे ध्यान देंगे?
वे अनुष्ठान तो करते हैं किन्तु अनेक ध्यान देने योग्य तथ्यों को नकार देते हैं जैसे शास्त्र के नियमों के अनुसार मन्त्र जप, देव-पूजन, दक्षिणा दान आदि। वे श्रद्धा और आदर से यज्ञ नहीं करते। उनकी इच्छा तो यह होती है कि लोग उन्हें 'सोमयाजी', सोम यज्ञ करने वाला कहें किन्तु उन्हें यज्ञ-फल की प्राप्ति नहीं होगी। उनमें सेवा भाव का अभाव होता है। वे श्रद्धा अथवा विश्वास से यज्ञ नहीं करते प्रत्युत् संसार को धोखा देने के लिए करते हैं।
मान-स्वयं को धन-ज्ञान आदि के कारण बड़ा समझ कर आदरणीय मानना, मान है।
मद-धन के नशे में चूर व्यक्ति गुरुजनों और विद्वज्जनों को भी घृणा की दृष्टि से देखता है। धन और ज्ञान से वे मदान्वित हो जाते हैं। और उनके सिर ही मानो घूम जाते हैं। यही मद है।
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः ।
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ।।१८ ।।
शब्दार्थ : अहंकारम्-मिथ्या अभिमान, बलम् बल, दर्पम् - दर्प (घमण्ड), कामम् -काम (विषय भोग), क्रोधम् -क्रोध, च-और, संश्रिताः-अवलम्बित, माम् -मुझे, आत्मपरदेहेषु-अपने और दूसरों के शरीरों में, प्रद्विषन्तः-द्वेष करते हुए, अभ्यसूयकाः - ईर्ष्यालु ।
अनुवाद : अहंकार, बल, अभिमान, काम और क्रोध के वश में हो कर ये ईर्ष्यालु लोग अपने तथा अन्य शरीरों में स्थित मुझ ईश्वर से ईर्ष्या करते हैं।
व्याख्या : वे आत्म निर्भर हैं और मानसिक तथा भौतिक शक्ति से गर्वान्वित हैं। वे अत्यधिक कृत्रिम जीवन जीते हैं। उन्हें कोई मान न दे तो कुपित हो उठते हैं। किसी भी अन्य वस्तु से अपना शरीर अधिक प्रिय है। वे केवल उसी के लिए जीवित रहते हैं। उनकी योजनाओं को यदि कोई व्यर्थ कर दे तो वे उसके प्रति कटुतापूर्वक उग्र हो उठते हैं। बदले की भावना से वे निर्दयतापूर्वक उसकी हिंसा कर देते हैं। वे अत्यन्त कृपण व अधम होते हैं। रात्रि के आगमन पर जैसे अन्धकार धीरे-धीरे बढ़ता है वैसे ही उनकी मूर्खता, उनका अहंकार, दर्प, मान, मोह दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु वे नृशंस शक्ति प्रयोग में लाते हैं। सत्यभाषी, दानी और मुझ में भक्ति भाव रखने वालों के साथ वे दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें अपशब्द कहते हैं।
अहंकारम् - मिथ्या अभिमान-आत्मोद्धत-तत्त्व, अविद्या का एक विकार अथवा कार्य है। यह मानव प्रकृति में और समस्त बुरे कर्मों में समस्त दोषों और अनर्थकारी विपरीत वृत्तियों का मूल स्रोत है। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान और दम्भ सब अहंकार के सेवक हैं। इस दुष्ट शत्रु को संयत करना अत्यन्त दुष्कर है। किन्तु विचारणा से इसका संहार हो सकता है।
अविद्यावश तथा मिथ्या रूप से अपने ऊपर आरोपित उत्कृष्ट गुणों के कारण ये असुर अत्यन्त अभिमानी होते हैं। स्वयं को गुण सम्पन्न मानने वाले ये सोचते हैं कि वे अत्यन्त महान हैं। मिथ्या रूप से आरोपित गुणों के कारण उनका अहंभाव भी और बढ़ जाता है। अपनी कोषजात (धन सम्बन्धी) वरीयता के कारण वे दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। निज स्वार्थपूर्ति हेतु अथवा झूठा प्रमाण (साक्ष्य) देने के लिए रिश्वत लेते हैं।
बलम् -काम और आसक्ति से युक्त शक्ति । असुर दूसरों को अपमानित करने अथवा नष्ट करने के लिए अपने बल का प्रयोग करते हैं। नैतिक पूर्णता लाने वाले पाँच विधान जो 'यम' के अन्तर्गत बताये गये हैं अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-यदि मनुष्य इनमें स्थित नहीं है, हृदय की शुद्धि नहीं है, उसका मन यदि अशुभ वृत्तियों से सिंचित है (पूर्ण है), और वह किसी प्रकार की शक्ति अर्जित कर लेता है तो वह उसका अनुचित प्रयोग करेगा और दूसरों को नीचा दिखाने व अपमानित करने का प्रयास करेगा। मन की एकाग्रता से सिद्धि और शक्ति प्राप्त होना निश्चित है। किन्तु यम-नियम का पालन करने वाला मनुष्य उनका अनुचित प्रयोग नहीं करेगा और उसका रहीं होगा। यही कारण है पतञ्जलि महर्षि ने कहा- "योग मार्ग में शक्तियाँ अवरोध उत्पन्न करती हैं। कठोरतापूर्वक उनको संयत करो । लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। भगवत्-चेतना की परमावस्था प्राप्त होने पर्यन्त, योग की सीढ़ी पर आरूढ़ रहो, जब तक तुम अन्तिम सोपान तक नहीं पहुँच जाते ।'' मुड़ कर मत देखो। बीते काल की स्मृतियों को विस्मृत कर दो।
यम योग की नींव है। ध्यानाभ्यास से पूर्व स्वयं को यम में स्थित करो। अनेक साधकों का पतन ही इसी कारण होता है कि वे यम का अभ्यास नहीं करते । प्रारम्भिक अवस्था में इसका अभ्यास अनिवार्य है जब कि वे सीधा ही ध्यान में बैठ जाते हैं। यह एक शोचनीय भूल है।
दर्प-मिथ्या अभिमान (जिसके कारण मनुष्य धर्म का भी अतिक्रमण कर जाता है) दर्प से युक्त हृदय वाला मनुष्य धृष्ट और अन्यायी बन जाता है और दूसरों के प्रति उद्धत और सगर्व शासन करने की वृत्ति अपना लेता है, वह गुरुजनों की अथवा अन्य अपने से बड़ों का आदर नहीं करता। यह एक विशेष दोष है जो उसके अन्तःकरण में घर कर लेता है। इस गुण की अभिव्यक्ति पर मनुष्य सदाचार से पथभ्रष्ट हो जाता है।
क्रोध-अप्रिय अथवा अरुचिकर समक्ष आने पर क्रोध की अभिव्यक्ति होती है।
ये असुर मुझ से द्वेष करते हैं। मैं इनके शरीरों में इनके विचारों और कर्मों का साक्षी द्रष्टा बन के वास करता हूँ। वे मुझे भी मानव समझ कर मुझ से घृणा करते हैं। वे मेरी सर्वव्यापक अनश्वर प्रकृति को नहीं समझ पाते। वेदों और स्मृतियों में दिये गये मेरे उपदेशों का और मेरी आज्ञा का वे अनुसरण नहीं करते । शास्त्र विहित उपदेशों का उल्लङ्घन करने वाला निश्चित रूप से मुझ से घृणा का कर्म कर रहा है। ये असुर, अत्यन्त ईर्ष्यालु होते हैं। उनकी वृत्ति और उनके उद्देश्य अशुभ होते हैं। धर्म के पथ पर आरूढ़ गुणी लोगों के प्रति वे द्वेष भाव रखते हैं। दूसरों के सद्गुणों को देख कर उनके हृदय स्पृहा से दीप्त होने लगते हैं। यह मात्सर्य है, एक प्रकार की ईर्ष्या है। यदि कोई मनुष्य किसी साधु पुरुष पर दुर्गुणों का अध्यास (आरोपण) करे, जो सद्गुणों से युक्त है, तो यह भाव असूया कहा जाता है। दूसरों की धन-सम्पत्ति और समृद्धि देख कर जलन हो तो उसे ईर्ष्या कहते हैं।
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ।।१९ ।।
शब्दार्थ : तान् उन, अहम् -मैं, द्विषतः द्वेष करने वालों को, क्रूरान् अत्याचारी, संसारेषु संसार में, नराधमान् नराधमों को, क्षिपामि गिराता हूँ, अजस्रम् सदा, अशुभान् -अशुभ, आसुरीषु-आसुरी, एव-ही, योनिषु योनियों में।
अनुवाद : उन क्रूर, ईर्ष्यालु, अशुभकर्मकारी नराधमों को संसार में सदा मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ।
व्याख्या : सब शरीरों के अन्तर्वासी मुझ ईश्वर से घृणा करने वाले, लोगों और पशुओं की हिंसा में प्रसन्न होने वाले, इन आसुरी मनुष्यों के साथ मैं कैसे बरतता हूँ, सुनो। मैं उन्हें मानव योनि से नीचे गिरा कर पशु आदि निम्न योनियों में भेज देता हूँ। मैं उन्हें व्याघ्र, सिंह, बिच्छु, साँप आदि क्रूर योनियों में गिराता हूँ।
'सदा' शब्द से यहाँ अभिप्राय है- जब तक वे अपने हृदय परिमार्जित नहीं कर लेते। शाश्वत निपतन जैसा कोई दंड नहीं है।
तान् - उन साधु पुरुषों से ईर्ष्या करने वाले और धर्म पथ पर आरूढ़ लोगों के शत्रु ।
नराधमान् -मनुष्यों में अधम, क्योंकि वे बुरे से बुरा कर्म करने के दोष से युक्त हैं और धार्मिक (सदाचारी) मनुष्यों को चोट पहुँचाने और गुणीजनों और मूक पशुओं की क्रूरतापूर्वक हिंसा करने में प्रमुदित होते हैं।
आसुरीषु योनिषु-असुरों की योनियों में। व्याघ्र और सिंह आदि की योनियाँ जो अत्यधिक क्रूर हैं।
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ।।२० ।।
शब्दार्थ : आसुरीम् - आसुरी, योनिम्-योनि को, आपन्नाः- प्राप्त हुए, मूढाः मूर्ख, जन्मनि जन्मनि-जन्मों-जन्मों में, माम् -मुझे, अप्राप्य-न पा कर, एव-ही, कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र, ततः-तत्पश्चात्, यान्ति-जाते हैं, अधमाम् -निम्नतर, गतिम् - गति को ।
अनुवाद : हे अर्जुन, आसुरी योनियों में प्रविष्ट हो कर और जन्म-जन्मान्तरों तक मोहित हुए ये मुझे न पा कर और निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं।
व्याख्या : ये पतित असुर राक्षसी योनियों में गिराये जाते हैं। वे अत्यन्त पतित और संत्रस्त अवस्था को पहुँचते हैं। घोर अन्धकार में उन्हें डाला जाता है। उनकी अत्यन्त तामसिक प्रकृति, पैशाचिक कर्म और इच्छाओं के कारण उन्हें निम्न से निम्नतम योनियाँ प्राप्त होती हैं। व्याघ्र की योनि के उपरान्त वे सर्पयोनि में प्रवेश करेंगे, सर्प से कीट योनि और इसके पश्चात् वृक्ष आदि योनि को प्राप्त होंगे। संस्कृत में 'तर' और 'तम' तुलनात्मक और सर्वोत्तम स्तर के लिए प्रयोग में आते हैं। ये असुर निकृष्टतम योनियों को प्राप्त होते हैं।
वे मुझ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनके अन्तःकरण अशुद्ध हैं क्योंकि वे धर्म पथ पर नहीं चलते और शास्त्रविहित उपदेशों और आदेशों का पालन नहीं करते । पैशाची प्रकृति आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वथा प्रतिकूल है (वैरी है)। अतः नियमित ध्यानाभ्यास और दिव्य गुणों का विकास कर के तुम्हें अशुभ वृत्तियों का निराकरण करना होगा। केवल तभी तुम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो।
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ।।२१ ।।
शब्दार्थ : त्रिविधम्-तीन प्रकार के, नरकस्य-नरक के, इदम् - यह, द्वारम् - द्वार, नाशनम् - विनाशकारी, आत्मनः- आत्मा के, कामः काम, क्रोधः क्रोध, तथा तथा, लोभः- लोभ, तस्मात्-इसलिए, एतत् यह, त्रयम्-तीन, त्यजेत्-त्याग देने चाहिए।
अनुवाद : आत्मा का विनाश करने वाले ये तीन प्रकार के दोष-काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। अतः इन तीनों अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए।
व्याख्या : काम, क्रोध और लोभ-ये महापथ के चोर मनुष्य को दुःख-क्लेश और नरक के अन्धकार से युक्त गभीरगर्त में गिराने वाले हैं। ये तीन कष्ट के उद्गम स्रोत हैं। ये तीन निम्नतम नरकों की ओर ले जाने वाले द्वार रूप हैं। ज्ञान, भक्ति और शान्ति के ये शत्रु हैं। इन अशुभ वृत्तियों के मन में प्रवेश करने पर मनुष्य अपना विवेक और मानसिक सन्तुलन खो बैठता है और अनेक बुरे कर्म करने लगता है।
काम, क्रोध और लोभ आत्मान्धता और अविद्या के सूचक हैं क्योंकि शुद्ध शाश्वत आत्म तत्त्व में अथवा ब्रह्म में विषय-वासना, अभाव, क्रोध, लोभ आदि विकारों का अभाव है।
नरकस्य द्वारम् नरक का द्वार। नरक की ओर ले जाने वाला द्वार। इस द्वार पर प्रवेश करते ही आत्मा का विनाश हो जाता है अर्थात् जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह संघर्ष अथवा पुरुषार्थ करने योग्य नहीं रहता।
यह द्वार क्योंकि आत्मा का हनन करने वाला है प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इन तीन का त्याग करे। (निरूपण - III.47)
इन तीनों का त्याग करने वाले मनुष्य की अगले श्लोक में प्रशंसा की गई है।
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ।।२२ ।।
शब्दार्थ : एतैः इनसे, विमुक्तः - मुक्त, कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र, तमोद्वारैः - अन्धकारमय द्वारों से, त्रिभिः-तीन (के द्वारा), नरः मनुष्य, आचरति-आचरण करता है, आत्मनः- आत्मा के, श्रेयः कल्याण का, ततः-तब, याति-जाता है, पराम् - परम, गतिम् - गति को (लक्ष्य को)।
अनुवाद : हे अर्जुन, अन्धकारमय इन तीन द्वारों से मुक्त हो कर मनुष्य आत्म कल्याण के लिए साधन करता है और इस प्रकार परम गति को प्राप्त होता है।
व्याख्या : नरक के इन तीन द्वारों का त्याग करने पर साधक के लिए मोक्ष का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। वह सन्तों का सान्निध्य प्राप्त करता है जो मोक्ष दिलाने वाला है। वह आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण कर के उन्हें अभ्यास में लाता है। वह शास्त्रों का श्रवण करता है, मनन करता है, ध्यान करता है और अन्त में आत्म साक्षात्कार कर लेता है।
तमोद्वार - अन्धकारमय द्वार जो नरक की ओर ले जाने वाले हैं जो कष्ट और भ्रान्ति से पूर्ण हैं।
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ।।२३ ।।
शब्दार्थ : यः जो, शास्त्रविधिम् - शास्त्र की विधि को, उत्सृज्य त्याग कर, वर्तते-कर्म करता है, कामकारतः-काम से प्रयुक्त हो कर, न-नहीं, सः वह, सिद्धिम् -सिद्धि, अवाप्नोति-प्राप्त करता है, न-नहीं, सुखम् -सुख, न नहीं, पराम् -परम, गतिम् गति ।
अनुवाद : वह जो शास्त्र की विधि को त्याग कर अर्थात् विधि-निषेध और विधिबोधक आदेशों का पालन न कर के कामना के वशीभूत हो कर कर्म करता है वह न तो सिद्धि (पूर्णता) प्राप्त करता है, न सुख और न ही परम गति को प्राप्त करता है।
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।।२४ ।।
शब्दार्थ : तस्मात् - इसलिए, शास्त्रम् - शास्त्र, प्रमाणम् -प्रमाण, ते-वे, कार्याकार्यव्यवस्थितौ -कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य की व्यवस्था में, ज्ञात्वा-जान कर, शास्त्रविधानोक्तम् - शास्त्र के विधान के अनुसार कही बात, कर्म-कर्म, कर्तुम् -करने के लिए, इह-इस लोक में, अर्हसि-योग्य हो, करना चाहिए।
अनुवाद : अतः कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण हैं। वेद शास्त्रों में विहित अध्यादेश का ज्ञान कर के तुम्हें इस संसार में कर्म करना चाहिए।
व्याख्या : आत्म कल्याण के इच्छुक मनुष्य को शास्त्र के आदेशों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। शाश्वत आनन्द प्राप्ति के जिज्ञासु को वेद और स्मृति ग्रन्थों का सम्मान करना चाहिए जो सदाचार के नियमों की नींव रखने वाले ग्रन्थ हैं। शास्त्रों में जिन बातों का निषेध हो उनका त्याग कर देना चाहिए और स्वीकार्य तथ्यों को ग्रहण करना चाहिए।
इस प्रकार पूर्ण रूपेण वेदों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति कभी दुर्भाग्य का सामना नहीं कर सकता। उसे शोक अथवा मोह नहीं हो सकता। इन शास्त्रों से बढ़कर कोई माँ इतनी दयालु नहीं हो सकती क्योंकि ये हमें बुरे कर्मों से बचा कर
हम पर परम श्रेय (मोक्ष) की वृष्टि करते हैं। इसलिए धर्मग्रन्थों का सम्मान करो। इनमें निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। जो कर्तव्य कर्म विहित हैं उन्हें पूर्ण हृदय और आन्तरिक बल से करो।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ।।१६ ।।
।। इति दैवासुरसम्पद्विभागयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथ सप्तदशोऽध्यायः
श्रद्धात्रयविभागयोगः
अर्जुन उवाच
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः ।
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ।।१ ।।
शब्दार्थ : ये-जो, शास्त्रविधिम् - शास्त्र की विधि को, उत्सृज्य-त्याग कर, यजन्ते-यज्ञ करते हैं, श्रद्धया-श्रद्धा से, अन्विताः- युक्त हो कर, तेषाम् - उनकी, निष्ठा-आस्था, तु-निश्चित रूप से, का-क्या, कृष्ण-हे कृष्ण, सत्त्वम् - सत्त्व, आहो-अथवा, रजः रजस्, तमः-तमस् ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे कृष्ण, शास्त्रों के विधि-विधान अथवा आज्ञा का व्यतिक्रम (उल्लंघन) कर के जो मनुष्य केवल श्रद्धापूर्वक देवादि पूजन करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? ये सात्त्विक है, राजसिक है अथवा तामसिक ?
व्याख्या : तीन प्रकार की निष्ठाओं से युक्त तीन प्रकार के मनुष्यों की प्रकृति का वर्णन इस अध्याय में निरूपित है। प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वाभाविक वृत्ति-सात्त्विक, राजसिक अथवा तामसिक के अनुरूप व्यवहार करता है।
अर्जुन कृष्ण से कहते हैं-"शास्त्रों का निगूढ़ अर्थ समझना अथवा ग्रहण करना अत्यन्त कठिन है और शास्त्रवेत्ता को प्राप्त करना और भी दुष्कर है जो वेदों का ज्ञान करा सके। अधिकांश मनुष्य पवित्र, सूक्ष्म, कुशाग्र और एकाग्र (अविचलित, स्थिर) बुद्धि से युक्त नहीं होते। जीवन की अवधि अल्प है। शास्त्र अनन्त हैं।
आध्यात्मिक पथ के प्रतिबन्धक अनेक हैं। ज्ञान प्राप्ति की सुविधा सर्वदा उपलब्ध नहीं होती। शास्त्रों में विरुद्ध भाव समक्ष आते हैं, उनका विरोध शमन करना है। आप कहते हैं कि शास्त्र-ज्ञान के बिना मोक्ष सम्भव नहीं है। एक साधारण मनुष्य, यद्यपि वह शास्त्र के उपदेशों को नहीं जानता तथापि दान करता है, यज्ञादि कर्म करता है, निष्ठापूर्वक भगवान् की पूजा करता है, सन्तों और ऋषि-मुनियों के चरणकमलों का अनुसरण करता है, वह एक बालक की भाँति है जो लिखित वर्णों का वैसे ही प्रतिलेखन (copy) करता है अथवा एक प्रज्ञाचक्षु किसी दृष्टिवान् से सहायता लेता है, हे भगवन्, कृपया बतायें उसकी निष्ठा किस प्रकार की है, सात्त्विक है, राजसिक है अथवा तामसिक? शास्त्रों का ज्ञान न रखने वालों की गति क्या है?
श्री भगवानुवाच
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ।।२ ।।
शब्दार्थ : त्रिविधा-तीन प्रकार की, भवति - होती है, श्रद्धा-श्रद्धा, देहिनाम् देहधारियों की, सा-वह (श्रद्धा), स्वभावजा - (उनकी) प्रकृति के अनुरूप, सात्त्विकी-सात्त्विकी, राजसी-राजसिक, च-और, एव-ही, तामसी-तामसिक, च-और, इति-इस प्रकार, ताम्-उसे, शृणु-सुनो।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : देहधारियों की स्वभावजन्य श्रद्धा तीन प्रकार की होती है-सात्त्विक (शुद्ध), राजसिक (आसक्तियुक्त), तामसिक (अन्धकारयुक्त) । अब इसके विषय में तुम मुझसे श्रवण करो।
व्याख्या : सम्पूर्ण जगत् मानो आस्थावान् है। तीन गुणों के प्रभाव से यह आस्था, श्रद्धा, तीन प्रकार की हो जाती है। सत्त्व का प्रबल विकास होने पर जब मनुष्य में सत्त्व का अतिरेक (आधिक्य) होता है तो उसके लिए आत्म-ज्ञान, आत्म-साक्षात्कार सहज हो जाता है। राजसी वृत्ति की प्रधानता से तो श्रद्धा क्रिया-कर्मों की चेटी (दासी) हो जाती है। तमस् का आच्छादन हो जाये तो श्रद्धा लुप्त हो जाती है।
सात्विक श्रद्धा से सम्पन्न व्यक्ति मोक्ष को अपना लक्ष्य मान कर आगे बढ़ते हैं। राजसिक मनुष्य सांसारिक क्रिया-कलापों अथवा क्षुद्र कर्त्तव्यों में संलग्न रहते हैं। तामसिक श्रद्धा वाले क्रूर प्रकृति के होते हैं। वे पशुबलि देते हैं। आत्माओं का आह्वान करते हैं, प्रेतों से प्रलाप करते हैं। श्रद्धा यदि सत्त्व-समन्वित हो जाये तो मोक्ष का साधन बन जाती है। राजसिक वृत्ति यदि प्रधान हो जाये तो श्रद्धा भी विविध-वर्ण युक्त हो कर विविध क्रियाओं में मनुष्य को संलग्न करती है। तमस् का अतिरेक (प्रधानता) होने पर तो समझ लो अन्धकार ही अन्धकार है। ज्ञान की किरण नहीं दिखेगी।
मनुष्य के मन के साथ मिल कर श्रद्धा पृथक् गुणों से सम्पन्न होती है। मन के अनेक रूप-रङ्ग हैं। मदिरा के पात्र में यदि गङ्गा-जल डाल दिया जाये तो वह दूषित हो जायेगा, इसी प्रकार दुर्जन की सङ्गति में सज्जन भी अवगुणों से युक्त हो जायेगा । तीन गुण मनुष्य की श्रद्धा पर अपना रङ्ग चढ़ाते रहते हैं अर्थात् उसके मन को प्रभावित करते रहते हैं। अन्य दो गुणों के दब जाने पर प्रधान गुण की अभिव्यक्ति के अनुरूप मानव मन कार्य करता है।
मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों के अनुरूप मन त्रिविध रूप धारण करता है। पूर्वजन्म के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का स्वभाव बनता है।
जैसी वृत्ति होती है, वैसी इच्छा उत्पन्न होती है, जैसी इच्छा होगी वैसा ही कर्म होगा, जैसा कर्म होगा मृत्यूपरान्त उसके अनुसार जन्म होगा। शरीर तो वृक्ष के बीज की भाँति है, एक अविच्छिन्न श्रृंखला है। वृक्ष के वृद्धिकाल में बीज का नाश होता है और वृक्ष पुनः नवीन बीज उत्पन्न करता है। सतत, शाश्वत रूप से यह क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य, देह धारण करता है, कर्म करता है, वृत्तियों का विकास करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और अपनी वृत्तियों के अनुरूप ही नव देह धारण करता है। जन्म-मृत्यु का मूल कारण अविद्या का जब तक विनाश नहीं होता और मनुष्य त्रिगुणातीत हो कर आत्म-ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यह क्रम चलता रहता है।
श्रद्धा स्वभावजन्य होती है अर्थात् पूर्व जन्मों में कृत शुभ-अशुभ कर्मों के सुप्त संस्कार जो मृत्यु के समय अभिव्यक्त होते हैं उनके समुदाय का नाम स्वभाव है। (उनसे उत्पन्न हुई श्रद्धा ही त्रिविध है।) चित्त में अथवा अवचेतन मन में पूर्व संस्कारों का मानो आगार है जो स्मृति से पुनर्जीवित होते हैं अर्थात स्मरण में आते हैं।
राजसिक-राक्षस और यक्षों की पूजा राजसिक है जो रजस् का प्रभाव है।
सात्त्विक-सत्त्व गुण से उत्पन्न हुई देव पूजादि विषयक श्रद्धा ।
तामसिक-तमोगुण से उत्पन्न प्रेतपिशाच आदि विषयक श्रद्धा तामसिक है जो तमोगुण का कार्य है।
श्रद्धा मनुष्य का प्रमुख अवलंबन है। यह मात्र बौद्धिक विश्वास अथवा प्रिय नीतियों का अन्धानुकरण नहीं है। इसकी विशेषताओं का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे तुम फल को देख कर वृक्ष की पहचान करते हो, वाणी से मानव मन की और सांसारिक सुख-दुःख के अनुरूप पूर्व कृत (जन्मान्तर) के कर्मों का ज्ञान करते हो इसी प्रकार श्रद्धा का भी स्पष्ट ज्ञान रखने का प्रयास करो।
स्वभावजा-स्वभावजन्य। पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न ।
तम् - उस । त्रिविध श्रद्धा की ओर संकेत है यहाँ ।
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः ।।३ ।।
शब्दार्थ : सत्त्वानुरूपा-स्वभाव के अनुरूप, सर्वस्य-सब की, श्रद्धा-श्रद्धा, भवति होती है, भारत- हे अर्जुन, श्रद्धामयः श्रद्धायुक्त, अयम्-यह, पुरुषः पुरुष, यः-जो, यच्छूद्धः- जैसी श्रद्धा, सः- वह, एव-ही, सः वह (है)।
अनुवाद : हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसकी प्रकृति के अनुरूप होती है। पुरुष श्रद्धामय है। जैसी जिसकी श्रद्धा है वह स्वयं भी वही है।
व्याख्या : प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा स्वभावजन्य होती है। मनुष्य श्रद्धा से अनुरंजित है। पूर्व श्लोक में 'स्वभाव' शब्द और इस श्लोक में 'सत्त्व' पर्यायवाची हैं।
मनुष्य के चरित्र की पहचान उसकी श्रद्धा से की जा सकती है। उसकी श्रद्धा उसके चरित्र का दर्पण है। श्रद्धा ने उसे जैसा बनाया है वही वह है। श्रद्धा से जीवन-चरित्र को स्वरूप दिया जा सकता है। श्रद्धा उसकी निष्ठा को इङ्गित करती है, उसका दोष निर्णय करती है। प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति, विशेष वृत्ति, संस्कार अथवा पूर्व जन्मों में किये गये अच्छे-बुरे कर्मों के सुप्त संस्कारों के पुनर्जागरण के अनुरूप होती है। प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा, अपना स्वरूप और गुण, उसके अस्तित्व की सामग्री, स्वभाव और संस्कारों से ग्रहण करती है।
सत्त्व-प्रकृति । स्वाभाविक अभिव्यक्ति, विशेष प्रकार की वृत्तियों से युक्त अन्तःकरण ।
सर्वस्य-प्रत्येक प्राणी की।
पुरुष-मनुष्य । आवागमन के चक्र में निगृहीत जीवात्मा । मन से प्रतिष्ठित आत्मा ।
श्रद्धामयः श्रद्धा से युक्त । अन्नमय कोष जैसे अन्न से पूर्ण है, आनन्दमय कोष आनन्द से पूर्ण है वैसे ही अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) श्रद्धा से पूर्ण है।
"पुरुष श्रद्धामय है, जैसी उसकी श्रद्धा है वही वह है।" यह सिद्धान्त अध्याय VII श्लोक २० और २३ तथा अध्याय IX श्लोक २५ में वर्णित की पुनरावृत्ति है।
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ।।४ ।।
शब्दार्थ : यजन्ते-पूजा करते हैं, सात्त्विकाः सात्त्विक, देवान् देवों की, यक्षरक्षांसि-यक्ष और राक्षसों का, राजसाः- राजसिक, प्रेतान् -प्रेत, भूतगणान् भूतों को, च - और, अन्ये-अन्य, यजन्ते-पूजते हैं, तामसाः-तामसिक, जनाः- लोग ।
अनुवाद : सात्त्विक, शुद्ध प्रकृति वाले पुरुष देवों का पूजन करते हैं। राजसिक अथवा मनोविकारी राग युक्त प्रकृति वाले यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं। तामसिक अथवा मोह ग्रस्त भूत-प्रेत आदि को पूजते हैं।
व्याख्या : श्रद्धा की परिभाषा बताने के उपरान्त भगवान् कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि श्रद्धा के अनुरूप पूजार्ह विषय का चयन कैसे होता है। श्री की प्रकृति (सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक) का अनुमान विशेष प्रमानों से किया जाता है जैसे देव पूजन आदि। प्रत्येक मनुष्य अपने अस्तित्व के प्रधान गुण के अनुरूप पूजा के विषय का चयन करता है। उसमें जिस गुण का अतिरेक होगा उसके अनुसार ही उसकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति होगी। सात्त्विक मनुष्य की श्रद्धा की अभिव्यक्ति सात्विक होगी, रजोगुण में स्थित मनुष्य की श्रद्धा राजसिक होगी और तमोगुण में स्थित मनुष्य की श्रद्धा की अभिव्यक्ति तामसिक होगी।
सात्त्विक पुरुष, सत्त्व भाव से युक्त और देव पूजन करने वाले इस संसार में विरल ही हैं।
यक्षगण कुबेर के बान्धव हैं। कुबेर धन के देवता हैं। भूत-पिशाच धन-सम्पत्ति की रक्षा करने वाले हैं।
राक्षस-बल और पराक्रम से युक्त जीव जैसे नैऋत (Nairrita), बृहत्काय राक्षस जो मायावी शक्तियों से युक्त होते हैं।
भूत-प्रेतनर, वेताल, निशाचर ।
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ।।५ ।।
शब्दार्थ : अशास्त्रविहितम्-शास्त्र में जिनका विधान नहीं है, घोरम् -घोर, तप्यन्ते-तप करते हैं, ये-जो, तपः-तप, जनाः मनुष्य, दम्भाहंकारसंयुक्ताः - दम्भ (घमण्ड) कामरागबलान्विताः-काम और राग (आसक्ति) से बलपूर्वक प्रेरित । और अहंकार से युक्त,
अनुवाद : वे मनुष्य जो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध घोर तप करते हैं, दम्भ और अहंकार से युक्त हैं और काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं,
व्याख्या : कुछ लोग सोचते हैं शरीर को कष्ट पहुँचाना लक्ष्य प्राप्ति का समुचित साधन है। अन्य लोगों को आकृष्ट कर के इन्द्रियों की तृप्ति के लिए धन अर्जित करना उनका ध्येय होता है। वे हाथ ऊपर उठा कर एक टाँग पर खड़े रहेंगे। यह कोई तपस्या नहीं है। यह तो तामसिक तपस् है। शारीरिक पीड़ा मोक्ष नहीं दिला सकती। ये लोग तो शास्त्रों के मूल तत्नों भी अनभिज्ञ हैं। विद्वानों की धार्मिक प्रक्रियाओं का वे उपहास करते हैं, वृद्ध जनों पर आक्षेप करते हैं। वे अपनी महानता के अभिमान में झूलते हैं। उन्हें अपनी सम्पदा का अहंकार है। वे शास्त्र द्वारा अप्रमाणित तपस्या करते हैं। अपने राग और इच्छा के बल पर वे अशास्त्रविहित घोर तप करते हैं।
अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए वे बच्चों की बलि चढ़ा देने में संकोच नहीं करते। अहंकार को न मार कर वे यज्ञ बलि के नाम पर निर्दोष पशुओं को मार डालते हैं। वस्तुतः अपनी रसना को सन्तुष्ट करने के लिए वे उन्हें मारते हैं। नृशंस कर्म ! शास्त्रों के विषय में वे अपशब्द कहते हैं और स्वयं मोह-ममता के वन में विचरण करते हैं। वे स्वयं भी दुःखी होते हैं और दूसरों को भी दुःख पहुँचाते हैं। वे ऐसी तपस्या करते है जो स्वयं उनके लिए भी कष्टप्रद है और दूसरों को भी (अन्य जीवों को) हानि पहुँचाने वाली है। शोचनीय है उनका भाग्य । उनका विनाश अपरिहार्य है।
कामरागबलान्विताः का अर्थ यह भी हो सकता है-काम, राग और बल से युक्त ।
दम्भ-आडंबर, दम्भी मनुष्य आकांक्षा करता है कि सब लोग उसे सज्जन मानें। वह वस्तुतः गुणी तो नहीं होता किन्तु वैसा होने का आडंबर करता है। जो वह नहीं है वह बनने या होने का बहाना करता है। मिथ्या अभिमान करता है।
अहंकार-अहंभाव । अहंकारी मनुष्य सोचता है और अनुभव करता है कि सभी सद्गुणों से वह युक्त है तथा अन्य लोगों से श्रेष्ठ है।
बल-ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग (आसक्ति) होने के कारण उग्र पीड़ा सहन करने की महान शक्ति। (पीड़ा जो पदार्थ की प्राप्ति और उसकी रक्षा में सहन करती पड़ती है) ।
काम-कामना। किसी भी विषय की कामना ।
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ।।६ ।।
शब्दार्थ : कर्षयन्तः कष्ट देते हुए, शरीरस्थम् - शरीर में स्थित, भूतग्रामम् - भूत समुदाय को (पंच तत्त्वों को), अचेतसः- अविवेकी, माम् मुझे, च और, एव-ही, अन्तःशरीरस्थम् - भीतर, शरीर में स्थित, तान् उन्हें, विद्धि-जानो, आसुरनिश्चयान् - असुर प्रवृत्ति वाले ।
अनुवाद : अविवेकी मनुष्य, शरीर में स्थित भूत समुदाय को तथा अन्तरात्मा में स्थित मुझे भी कष्ट पहुँचाते हैं, उन्हें तुम आसुरी संकल्पों वाला जानो ।
व्याख्या : भूत ग्रामम् समस्त तत्त्वों का समुदाय जो शरीर का निर्माण करता है।
(भूत) ग्रामम् - इन्द्रियादि करणों के रूप में परिणत भूत समुदाय को।
माम् -मुझ को। वासुदेव को जो उनके कर्मों और विचारों का साक्षी है।
मुझे इस प्रकार कष्ट देने वाला मेरे उपदेशों की पूर्णतया अवहेलना (अवज्ञा) करता है।
अचेतसः- बुद्धिहीन, अचेत, विवेकशून्य ।
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ।।७ ।।
शब्दार्थ : आहारः - भोजन, तु-वस्तुतः, अपि-भी, सर्वस्य-सब का, त्रिविधः-तीन प्रकार का, भवति-होता है, प्रियः-प्रिय, यज्ञः यज्ञ, तपः-तप, तथा-और, दानम् दान, तेषाम् - उनके, भेदम्-भेद, इमम् - यह, शृणु-सुनो।
अनुवाद : भोजन भी जो सबको प्रिय है, तीन प्रकार का है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान की क्रियायें भी त्रिविध हैं। इनके भेद अब सुनो।
व्याख्या : सर्वस्य-प्रत्येक का अर्थात् आहार लेने वाले सब प्राणी ।
इमम् - इसको, जो बताने लगे हैं।
तेषाम् उनका अर्थात् भोजन आदि का।
गुणों के अनुसार मनुष्य के आहार-विशेष का स्वरूप निश्चित होता है। आहार तीन प्रकार का है जो मनुष्य ग्रहण कर सकता है।
प्रत्येक आहार का अपना एक गुण होता है। मस्तिष्कीय कोषों पर पृथक् पृथक् प्रकार के आहार पृथक् प्रभाव डालते हैं। गौरैया, माँस, मछली, अण्डा, प्याज और लहसुन उत्तेजक भक्ष्य पदार्थ हैं। फल, जौ आदि मन शान्त और सौम्य बनाते हैं। आहार की प्रकृति मानव मन को प्रभावित करती है। अपने स्वभाव अथवा गुण के अनुरूप मनुष्य आहार-विशेष की अभिलाषा करता है।
शरीर रूपी उपकरण के द्वारा मनुष्य संसार में समस्त कार्य निष्पन्न करता है। यह शरीर मानो अश्व है जो मनुष्य को अपने लक्ष्य (मोक्ष) तक पहुँचाता है। अतः इसे शुद्ध-पवित्र, स्वस्थ और शक्तिसम्पन्न रखना चाहिए। क्रियाओं को स्वरूप देने के लिए शरीर, मन द्वारा निर्मित साँचा है। मन और शरीर में निकट का सम्बन्ध है। शरीर की दशा और प्रकृति का मानसिक प्रक्रियाओं पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। इसलिए शरीर और मन का निर्माण करने वाले भक्ष्य पदार्थ
पवित्र, पोषक, सौम्य, सात्त्विक, मधुर (कोमल) तथा आरोग्यावह होने चाहिए। इस संसार में प्रत्येक वस्तु त्रिविध है। आहार अपने-अपने लक्षणों और शरीर तथा मन पर डालने वाले प्रभावों के कारण सात्त्विक, राजसिक अथवा तामसिक हैं। मनुष्य जो आहार लेता है उससे उसके स्वभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। तुम अपनी प्रकृति को जान सकते हो कि वह सात्त्विक है, राजसिक है अथवा तामसिक । आहार विशेष के प्रति तुम्हारी रुचि के अनुसार यह अनुमान तुम लगा सकते हो और इसके पश्चात् राजसिक और तामसिक आहार का त्याग कर के सात्त्विक आहार का सेवन करो।
यज्ञ, तपस् और दान में त्रिविध विभाग क्यों हैं? क्योंकि यह त्रिविध विभाग गुणों की प्रकृति के अनुरूप है। राजसिक और तामसिक गुणों की खोज करो, उनका त्याग करो और पूर्ण रूप से सात्त्विक प्रवृत्ति अपनाओ।
कृच्छू और चान्द्रायण व्रतों का अभ्यास शरीर को तथा इन्द्रियों को क्षीण करता है, यह तप है। ध्यान भी तप है। यह मुखाकृति को ब्रह्म तेज, दिव्य आभा और आलोक से युक्त करता है।
आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ।।८ ।।
शब्दार्थ : आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः- आयु, सत्त्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति (हर्ष और पाचन शक्ति) बढ़ाने वाले, रस्याः रस युक्त, स्निग्धाः-चिकने, स्थिरा:-पोषक, हृद्याः रुचिकर, आहाराः भोज्य पदार्थ, सात्त्विकप्रियाः सात्त्विक मनुष्य को प्रिय हैं।
अनुवाद : आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य (आरोग्यता), सुख और प्रीतिवर्धक खाद्य पदार्थ जो रसयुक्त, स्निग्ध (चिकने), स्थिर (पोषक) और रुचिकर हैं, वे सात्त्विक मनुष्य को प्रिय हैं।
व्याख्या : शुद्ध सात्त्विक भोजन प्राण शक्ति और बल प्रदायक हैं। यह मानसिक शक्ति का भी विकास करने वाले हैं।
सत्त्व-प्रसन्नता, शुद्धता, आन्तरिक-नैतिक-आध्यात्मिक शक्ति और बल जो मन को अवसाद के क्षणों में स्थिर रखता है।
बल-शक्ति, कठिन कार्य करने पर भी थकावट न होना।
प्रीति-ओकाई (वमन) का अभाव, अच्छी पाचन शक्ति ।
रस्याः - मधुर और रसयुक्त ।
स्थिराः-पोषक, जो दीर्घावधि तक शरीर में (सार रूप से) रह सकते हैं। ये शक्तिप्रद हैं किन्तु पाचन में कठिनाई नहीं करते।
हृद्या:-आहार पर एक दृष्टि ही मन को सुखद हो और धुँए की गन्ध से और दग्ध-अवस्था से मुक्त हो।
सात्त्विक भोजन प्रसन्नता, सौम्यता और मानसिक स्पष्टता प्रदान करने वाला होता है। यह साधक को गहन ध्यान में प्रवेश करने, मानसिक शान्ति और सन्तुलन बनाये रखने में सहायक है। इस से शरीर और मन को सर्वाधिक शक्ति प्राप्त होती है। यह सहज रूप से पच कर समीकरण को प्राप्त होता है।
सात्त्विक मनुष्य को रसयुक्त आहार तथा अन्य आहार जो रूप में आकर्षक, स्पर्श में कोमल, स्वाद में रुचिकर, परिमाण में कम, पोषक अधिक हों-प्रिय हैं। इनकी तुलना आध्यात्मिक गुरु के मुखारविन्द से निःसृत वचनों से की जाती है जो कम होते हुए भी अत्यन्त मार्मिक और सारगर्भित होते हैं। सात्त्विक आहार आरोग्यता की दृष्टि से अत्यन्त अनुकूल होता है।
सत्त्व वृद्धि करने वाले आहार का सेवन करो। दुग्ध, नवनीत, ताजा पके फल, बादाम, हरी दाल, जौ, परवल, तोरई, करेला, कदली (केला) आदि सात्त्विक हैं। माँस, मछली, अण्डा, मदिरा का क्रूरता से त्याग करो यदि तुम सत्त्व वृद्धि कर के मोक्ष प्राप्ति चाहते हो तो । भोजन के सूक्ष्मतम भाग से मन बनता है, तभी तो कहा जाता है- "जैसा अन्न वैसा मन" । यदि तुम सात्त्विक भोजन करते हो तो मन भी सात्त्विक होगा। शरीर के सप्त धातु (सार रूप मूल तत्व) त्वचा, रक्त, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य भोजन से बनते हैं।
इन सप्त धातुओं के सदृश (अनुरूप) मन में विचार उत्पन्न होते हैं। इन तत्त्वों की जैसी दशा होगी वैसा ही मन बनेगा। जल से भरा हुआ पात्र अग्नि पर रखा जाये तो जल उष्ण हो जायेगा। वैसे ही मन की संरचना और प्रकृति भी भोजन अथवा सप्तधातु की संरचना और प्रकृति सदृश होगी।
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।।९ ।।
शब्दार्थ : कट्द्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीक्ष्ण (तीखे), रूक्ष (रूखे), दाहकारक, आहाराः - भोजन, राजसस्य-रजस् गुण वाले को, इष्टाः रुचिकर, दुःखशोकामयप्रदाः- दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले।
अनुवाद : कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष और दाहकारक आहार दुःख, शोक और रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं तथा राजसी प्रकृति के मनुष्यों को प्रिय हैं।
व्याख्या : अति शब्द सभी सात गुणों के साथ जोड़ना चाहिए जैसे अति कटु, अति लवण युक्त आदि।
राजसिक भोजन मन में अशुभ विचार, उत्तेजना, अन्य-अन्य वस्तुओं की तृष्णा, दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। राजसिक मनुष्य अपनी रसना को सन्तुष्ट करने के लिए सदा विभिन्न प्रकार के व्यञ्जन बनाने की योजना बनाता रहता है। वह नमक, मिर्च, तेल, लवंग, मसाले, खट्टे अचार आदि अधिकता में सेवन करता है। उसके नेत्रों से पानी बहने लगे अथवा नासिका से बूँदें टपकने लगें फिर भी वह उष्ण और खट्टे पदार्थों का त्याग नहीं करता। जब तक जिह्वा मिर्च से जलने न लगे, खट्टे पदार्थों से उदर पूर्ण रूप से भर न जाये उसका तालु (palate) असन्तुष्ट रहता है। भिंडी, पूरी, कचौरी, खट्टे मसाले, माँस, मछली, अण्डा, मिठाई, आलू, तली हुई ब्रैड, दही, बैंगन, गाजर, काला चना, प्याज, लहसुन, नींबू, मसूर, चाय, काफी, पान, तम्बाकू-ये सब आहार में राजसिक पदार्थ हैं।
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ।।१०।।
शब्दार्थ : यातयामम् -सत्त्व रहित, गतरसम्-नीरस, पूति-दुर्गन्धयुक्त, पर्युषितम्-बासी, रात्र्यंतरित (जिसको पके हुए एक रात बीत गई हो),च - और, यत् -जो, उच्छिष्टम् बचा हुआ (खाने के पश्चात् बचा), अपि-भी, च - और, अमेध्यम् अपवित्र, भोजनम् - भोजन, तामसप्रियम् - तामसी मनुष्यों को प्रिय।
अनुवाद : जो आहार सत्त्व रहित, नीरस, दुर्गन्धयुक्त, बासी, झूठा (बचा हुआ), अपवित्र हो वह तामसिक मनुष्यों को प्रिय है।
व्याख्या : गांजा (cannabis indica), भांग, अहिफेन (opium), कोकीन (cocaine), चरस, चन्डू (chandoo), ये सब सत्त्व रहित और दुर्गन्धयुक्त पदार्थ हैं और तामसिक हैं।
यातयामम् - इसका शाब्दिक अर्थ है तीन घण्टे पूर्व पकाया गया। '
यातयामम्' और 'गतरसम्' पर्यायवाची हैं।
पर्युषितम् दुर्गन्धयुक्त । पका हुआ रात भर का रखा भोजन ।
उच्छिष्टम् - भोजनोपरान्त थाली में बचा भोजन ।
तामसिक वृत्ति का मनुष्य एक दिन पूर्व का बना भोजन दूसरे दिन मध्याह्न में खायेगा। वह अधपका अथवा अधिक पका (जला हुआ) भोजन भी स्वाद से सेवन करता है। भोजन जब तक बासी और खट्टा न हो जाये तब तक वह सेवन नहीं करता। वह निषिद्ध पेय और खाद्य पदार्थों को लेता है। वह मदिरा पान करता है, ताड़ी (शर्बत मिली मदिरा) जो खट्टी हो चुकी है उसका सेवन करता है। राक्षसी वृत्ति से युक्त यह अत्यन्त भयावह होता है।
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।।११।।
शब्दार्थ : अफलाकाचिभि:- फल की इच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा, यज्ञः-यज्ञ, विधिदृष्टः-शास्त्रों के निर्देशानुसार, यः-जो, इज्यते-किया जाता है, पटव्यम् - यज्ञ सम्पन्न होना चाहिए, एव-ही, इति-इस प्रकार, मनः- मन, समाधाय-स्थिर करके, सः वह, सात्त्विकः सात्त्विक ।
अनुवाद : वही यज्ञ सात्त्विक है जो निष्काम भाव से युक्त पुरुषों द्वारा विधि-विधान से युक्त अर्थात् शास्त्र के निर्देशानुसार अपना कर्तव्य कर्म समझ कर किया जाता है।
व्याख्या : जब कोई यज्ञादि कर्म पूर्ण सात्त्विक भाव, निष्ठा और भक्ति से, निष्काम भाव से, अनन्यमनस्क हो कर और अपना कर्त्तव्य कर्म समझ कर किया जाता है तो वह कर्म सात्त्विक (शुद्ध) प्रकृति का कहा जाता है। यह अनुष्ठान निष्काम भाव से केवल आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के साधन रूप में सम्पन्न किया जाता है। मनुष्य की सात्त्विक प्रकृति ही उसे बिना किसी कामना के निःस्वार्थ भाव से कर्म करने को बाधित करती है। वह अपने मोक्ष की भी कामना नहीं करता प्रत्युत् इसलिए करता है कि वह कर्त्तव्य कर्म है और अवश्य किया जाना चाहिए। वह कृत संकल्प होता है कि यज्ञ एक कर्त्तव्य है और पूर्ण होना चाहिए।
यज्ञ का अर्थ यहाँ नैमित्तिक यज्ञ से नहीं है। यह विशाल अर्थ में प्रयोग होता है। कोई भी कर्म जो निःस्वार्थ भाव से, कामना रहित, आसक्ति रहित, अहंभाव रहित, फलाकाङ्क्षा रहित ईश्वर को समर्पित कर के किया जाये वह यज्ञ है।
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ।।१२ ।।
शब्दार्थ : अभिसंधाय-इच्छा कर के, तु-वस्तुतः, फलम् -फल, दम्भार्थम् - अभिमान के लिए, अपि-भी, च-और, एव - ही, यत्-जो, इज्यते-अर्पित किया जाता है, भरतश्रेष्ठ- हे भरतश्रेष्ठ (अर्जुन), तम्-उस, यज्ञम् यज्ञ को, विद्धि-जानो, राजसम् -राजसिक ।
अनुवाद : हे अर्जुन, जो यज्ञ फल की आकाङ्क्षा से अथवा मिथ्या अभिमान वश किया जाता है उसे राजसिक जानो ।
व्याख्या : पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा अथवा नाम और ख्याति के लिए किया गया यज्ञ राजसिक होता है। इस प्रकार का यज्ञकर्ता अपना महत्त्व बढ़ाने के लिए, विश्वविख्यात होने के लिए, परिणाम में कुछ फल प्राप्त करने के लिए, स्वयं को महान दर्शाने के लिए, पावन और शिक्षित विद्वान सा दिखने का आडंबर रचाने के लिए और अपनी ही महिमा का गुणगान करवाने हेतु अपी सम्पदा का प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ करता है। उसमें आत्म-ज्ञान की अभिलाषा कदापि नहीं होती।
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ।।१३ ।।
शब्दार्थ : विधिहीनम् - शास्त्र विधि से रहित, असृष्टान्नम् - बिना प्रसाद वितरण किये, मन्त्रहीनम् मन्त्रोच्चारण किये बिना, अदक्षिणम् - दक्षिणा रहित, श्रद्धाविरहितम् श्रद्धारहित, यज्ञम्-यज्ञ, तामसम्-तामसिक, परिचक्षते-कहा जाता है।
अनुवाद : वह यज्ञ तामसिक माना जाता है जो शास्त्र विधि के विपरीत हो, प्रसाद रहित हो, मन्त्र रहित हो, दक्षिणा रहित हो और श्रद्धारहित हो।
व्याख्या : तामसिक मनुष्य के द्वारा यज्ञ शास्त्र-निर्देशों के सर्वथा विपरीत होता है, उसमें मन्त्रों का प्रयोग नहीं होता। इस यज्ञ में हर प्रकार की अनियमितता देखी जा सकती है। अन्न का प्रसाद वितरित नहीं होता। शास्त्र के निर्देश के अनुसार पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी जाती । मन्त्रोच्चारण यथार्थ नहीं होता । स्तोत्र गान, उच्चारण और छन्द भी दोषयुक्त होता है। कभी-कभी तो गान होता ही नहीं। श्रद्धा का नितान्त अभाव रहता है। ऐसा यज्ञ करने वाला मनुष्य कोई लाभ प्राप्त नहीं करता ।
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ।।१४ ।।
शब्दार्थ : देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् -देव, द्विज (ब्राह्मण), गुरु और विद्वान् की पूजा, शौचम् - शुद्धि, आर्जवम् -सरलता, ब्रह्मचर्यम् ब्रह्मचर्य, अहिंसा- अहिंसा, च-और, शारीरम्-शरीर का, तपः-तप, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : देव, द्विज, गुरु और पूज्य व्यक्ति की पूजा, शुचिता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप कहे जाते हैं।
व्याख्या : तपस् -तप, आत्मानुशासन ।
चरणों का उपयोग तीर्थ में पावन मन्दिर में जाने के लिए हो, हस्त मन्दिर की स्वच्छता में लगें, भगवान् की पूजा की सामग्री एकत्र करने में लगें और अर्चन-वन्दन में लगे । ब्राह्मणों, गुरुजनों और विद्वानों को साष्टाङ्ग प्रणाम और ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन-ये शारीरिक तप हैं। शरीर का उपयोग माता-पिता और गुरु तथा दीन-दुःखी रोगी की सेवा में है। यह भी शारीरिक तप है। शरीर के द्वारा किया जाने वाला तप शारीरिक तप है। ऐसे तप करने के लिए शरीर ही साधन है। इसीलिए यह शारीरिक तप कहलाता है। चोरी न करना (अस्तेय) और दूसरे के धन का लालच न करना भी शारीरिक तप है।
जिसने ब्रह्म-साक्षात्कार कर लिया है वह प्रज्ञावान् है। कोई शूद्र भी प्रज्ञावान् हो सकता है। विदुर शूद्र होते हुए भी ज्ञानी था। इसी कारण से भगवान् ने प्रज्ञावान् का संकेत पृथक् रूप से किया है।
ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम (मैथुन में रत न होना)। यहाँ उस वृत्ति को संयत करने के अर्थ में है, दबाने में नहीं। यदि मन ध्यान, जप, प्रार्थना, शास्त्राध्ययन, आत्मविश्लेषण और "मैं कौन हूँ" के भाव से पूर्ण होगा और रतिभाव से शून्य शुद्ध आत्म तत्त्व का चिन्तन करेगा तो मन के प्रत्याहरण के साथ ही सम्भोग की इच्छा भी शिथिल हो कर समाप्त हो जायेगी। मन तनु (सूक्ष्म) हो जायेगा। कामेच्छा यदि दबा दी जाये तो यह पुनः-पुनः आक्रमण कर के मन को अशान्त और उत्तेजित करेगी और इससे वीर्य स्खलन होगा। ध्यान, जप, भगवन्नाम संकीर्तन और प्रार्थना से मन को शुद्ध रखना चाहिए। प्रथम तो मन का संयम अनिवार्य है। इसके उपरान्त इन्द्रियों का संयम सहज हो जायेगा। यही कारण है कि षट् सम्पत् में शम (मन का संयम) प्रथम स्थान पर है और दम (इन्द्रियों का नियन्त्रण) द्वितीय स्थान पर आचक्षित है। मन की सहायता के बिना इन्द्रियाँ चेष्टा नहीं कर सकीं। इसलिए कामेच्छा का प्रभावशील उपचार और ब्रह्मचर्य का श्रेष्ठ साधन है मन का नियन्त्रण एवं तदुपरान्त इन्द्रिय निग्रह ।
इन्द्रिय-विषयों का अत्यधिक चिन्तन वास्तविक इन्द्रिय-तुष्टि की अपेक्षा आन्तरिक आध्यात्मिक जीवन को अधिक हानि पहुँचाता है। साधना से यदि मन पवित्र नहीं किया तो मात्र इन्द्रियों का बाह्य नियन्त्रण अपेक्षित फल देने में असमर्थ होगा। यद्यपि बाह्य इन्द्रियाँ निग्रहीत हों तथापि उनके आन्तरिक प्रतिरूप जो अभी बलवान और उग्र हैं, मन से बदला लेते हैं और उग्र मनोद्वेग तथा वन्य संकल्पनाओं को जन्म देते हैं।
"अहो चेष्टाप्रतिरूपिका कामिनो मनोवृत्तिः।"
-शाकुन्तलम्
नवसाधकों के लिए मनोनिग्रह दुष्कर है। यदि इन्द्रियों को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये तो मन को, निग्रह करना कठिन हो जायेगा। इसी कारण भगवान् कृष्ण कहते हैं- "इसलिए हे अर्जुन! इन्द्रियों को पहले वशीभूत करके जान और विवेक को नष्ट करने वाले काम को मार डालो।" (निरूपण - III.41)
मन को प्रथम संयत करने का सिद्धान्त उचित है। यह अभ्यास प्रथम श्रेणी के साधकों के लिए हितकर है। मध्यम श्रेणी के साधकों को प्रथम इन्द्रिय-निग्रह करना होगा । इन्द्रियों की वृत्ति बहिर्मुखी होती है। मन इन्द्रियों के माध्यम से कार्य करता है। एक को संयत करने पर दूसरा भी संयत हो जाता है। इन्द्रिय संयम का अभिप्राय मन का संयम भी है क्योंकि मन इन्द्रियों का पुंज (समूह) ही है। इन्द्रियाँ न हों तो मन भी न हो।
शत्रु पर यदि दोनों अग्र भागों से आक्रमण किया जाये तो शत्रु पर विजय हो सकती है। इसी प्रकार मन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है यदि दो अग्र भागों से यौगपदिक (सहज ही) आक्रमण किया जाये-इन्द्रियों पर बाह्य आक्रमण और मन पर आन्तरिक आक्रमण जो कि इच्छाओं, कामनाओं के निराकरण द्वारा सम्भव है।
मन को प्रथम संयत करो, ऐसा कहा जाये तो तुम प्रथम इन्द्रियों को संयत करो-यह एक विचारधारा है। दूसरी विचारधारा है-इन्द्रियों को पहले वश में करो, मन सहज ही वशीभूत हो जायेगा। ये तर्क व्यर्थ ही पापवृत में फंसाने वाला है जैसे-“वृक्ष का अस्तित्व प्रथम था अथवा बीज का" अथवा "तुम आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लोगे यदि तुम समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लो-और तुम कामनाओं पर संयम तभी कर सकते हो जब तुम्हें आत्म-ज्ञान होगा।"
इस असत्यभासित तथ्य को देख कर तुम्हें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों में से एक का अभ्यास करने का यत्न करो अर्थात् अपनी रुचि, सामर्थ्य और प्रकृति के अनुसार मनोनिग्रह अथवा इन्द्रिय-निग्रह करो। अभ्यास द्वारा तुम स्वयं ही जान जाओगे, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। अभ्यास में आगे बढ़ने पर शनैः-शनैः शंकायें दूर होती जायेंगी और तुम परम सुख और शान्ति का आनन्द लोगे ।
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।। १५ ।।
शब्दार्थ : अनुद्वेगकरम् - उद्वेग (दुःख) न करने वाले, वाक्यम् वचन, सत्यम् -सत्य, प्रियहितम् - प्रिय और हितकर, च - और, यत्-जो, स्वाध्यायाभ्यसनम् वेदाध्ययन का अभ्यास, च-और, एव-ही, वाङ्मयम् - वाणी का, तपः-तप, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : उद्वेग न लाने वाले, सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलना तथा वेदों का अभ्यास-ये वाणी के तप कहे गये हैं।
व्याख्या : वाणी का तप करने वाले मनुष्य के वचन किसी के लिए दुःखकर नहीं हो सकते। उसके वचन दूसरों को सान्त्वना और हर्ष प्रदान करने वाले होंगे। उसके शब्द सब के लिए हितकारी होंगे। वाणी मन को विक्षिप्त (भ्रमित) भी कर सकती है। वाणी का संयम एक कठिन अनुशासन है किन्तु परम शान्ति के इच्छुक साधकों को इसका अभ्यास करना होगा। दृढ़ संकल्प, सहिष्णुता, कार्य में सत्य बर्ताव (ईमानदारी), और सतत प्रयास में रत साधक के लिए कुछ भी असम्भव नहीं है।
मनुस्मृति में कहा है-“सत्य भाषण करो, असत्य भाषण मत करो, सत्य किन्तु अप्रिय मत बोलो। प्रिय वचन हो और सत्य न हो तो भी मत बोलो। यही सनातन धर्म है।"
“सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः ।।"
उद्वेगकरम् -जीवों को दुःख देने वाले ।
वाङ्मयम् - वाणी का तप वही है जो इस श्लोक में वर्णित सभी गुणों से युक्त हो अर्थात्, अनुद्वेगकर (किसी को कष्ट न पहुँचाने वाला), सत्य, प्रिय और हितकर वचन । यदि इनमें से कोई एक भी अभाव में हो, शेष तीन हों तो इसे वाणी का तप नहीं समझना चाहिए। वाणी प्रिय तो है किन्तु अन्य तीन लक्षण (अनुद्वेगकर, सत्य और हितकर) इसमें विद्यमान नहीं हैं तो इसे वाणी का तप नहीं कहा जा सकता ।
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।।१६ ।।
शब्दार्थ : मनःप्रसादः मन की सौम्यता, शान्ति, सौम्यत्वम् - अन्तःकरण की शुद्धवृत्ति, मौनम् -मौन, आत्मविनिग्रहः- आत्म संयम, भावसंशुद्धिः विभाव में निर्मलता, इति-इस प्रकार, एतत्-यह, तपः-तप, मानसम् -मानसिक, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : मन की प्रशान्तता, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और मन की निर्मलता-यह मानसिक तप कहा जाता है।
व्याख्या : ऊर्मियों से रहित सरोवर जैसे सतह में अत्यन्त शान्त होता है वैसे ही विकार रहित मन जो इन्द्रिय-विषयों में भटकने वाला न हो, अत्यन्त प्रशान्त और सौम्य होता है।
सौम्यत्वम् -सब प्राणियों के कल्याण का भाव रखना।
यह मन की एक अवस्था है जो अपने प्रभाव, मुख के तेज आदि से अनुभव की जा सकती है।
मौनम् वाणी का मौन भी विचार संयम के लिए अनिवार्य है, अतः यहाँ कार्य रूप को कारण के पीछे प्रयोग किया गया है अर्थात् विचार-निग्रह। यह विचार को संयत करने का ही परिणाम है कि वाणी मौन है, मन भी मौन है, विचलित कर देने वाली बाह्य स्थितियों के रहते भी मन शान्त है, मौन है। मौन मुनि (ज्ञानी) की अवस्था है, अनन्यमनस्क ध्यान ।
आत्मविनिग्रहः - आत्म संयम अर्थात् अन्तःकरण अथवा मन का संयम । असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था जिसमें सब मनोवृत्तियाँ संयत रहती हैं। मन इन्द्रियों के पीछे और इन्द्रियाँ विषयों के पीछे नहीं भाग सकतीं। जहाँ तक वाणी का प्रश्न है, मौन, विचारों का संयम है।
भावसंशुद्धिः - अन्तःकरण की शुद्धि । ईमानदारी, छलकपट का अभाव, मन की वह अवस्था जिसमें काम, क्रोध, लोभ आदि नहीं होते।
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः ।
अफलाकाङ्गिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ।।१७।।
शब्दार्थ : श्रद्धया-श्रद्धा से, परया-परम, तप्तम् - अभ्यास किया गया, तपः-तप, तत्-वह, त्रिविधम्-तीन प्रकार का, नरैः- मनुष्यों द्वारा, अफलाकांक्षिभि -फल की इच्छा न चाहने वाले, सात्विकम् -युक्तैः युक्त, सात्विक, परिचक्षते-कहा जाता है।
अनुवाद : यह तीन प्रकार का तप जिसका अभ्यास-युक्तचित्त वाले पूर्ण श्रद्धा और निष्काम भाव से करते हैं, सात्त्विक तप कहलाता है।
व्याख्या : त्रिविधम्-तीन प्रकार का-कायिक, वाचिक और मानसिक ।
युक्तैः समाहित, युक्त । सन्तुलित मन, सफलता और असफलता में सम (अप्रभावित) ।
श्रद्धया श्रद्धा से, विश्वास से। परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास, गुरु के वचनों में विश्वास, शास्त्र के वचनों में विश्वास और स्वयं अपनी आत्मा में विश्वास । 1
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ।।१८ ।।
शब्दार्थ : सत्कारमानपूजार्थम् -सत्कार, मान और पूजा के उद्देश्य से, तपः-तप, दम्भेन-मिथ्याभिमान द्वारा, च-और, एव-ही, यत्-जो, क्रियते-किया जाता है, तत्-वह, इह-इस लोक में, प्रोक्तम् -कहा गया है, राजसम् -राजसिक, चलम् - अस्थिर, अध्रुवम् क्षणिक ।
अनुवाद : जो तप सत्कार, मान और पूजा के भाव से तथा मिथ्या अभिमान वश किया जाता है वह राजसिक तप है जो अस्थिर एवं क्षणिक है।
व्याख्या : वह तप जो श्रद्धायुक्त नहीं होता, मात्र आडंबर होता है, अपना महत्त्व बढ़ाने के लिए होता है ताकि लोग तप करने वाले को मान- सम्मान प्रदान करें, उसका गुणगान करें, राजसिक प्रकृति का कहा गया है।
इह-इस लोक में। ऐसा तप केवल इस भौतिक लोक में फल प्रदान करने वाला होता है।
सत्कार-अच्छा स्वागत, इन शब्दों में-"यह महान तपस्वी ब्राह्मण है।"
मान-मान, आदर। अपने स्थान से उठ कर स्वागत करना और सम्मानपूर्वक प्रणाम करना।
चलम् - अस्थिर, क्षणिक प्रभाव वाला ।
अध्रुवम् -बिना किसी नियम के, अस्थिर ।
ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया तप सर्वथा व्यर्थ है। इसका कोई परिणाम नहीं। अधूरा होने पर भी इसका त्याग कर दिया जाता है जब यह समझ आता है कि इसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा।
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ।।१९ ।।
शब्दार्थ : मूढग्राहेण-अविवेकपूर्ण निश्चय से, आत्मनः- अपने आप को, यत्-जो, पीडया-कष्ट से, क्रियते-किया जाता है, तपः-तप, परस्य-अन्य को, उत्सादनार्थम् नष्ट करने के लिए, वा-अथवा, तत्-वह, तामसम् - तामसिक, उदाहृतम्-कहा जाता है।
अनुवाद : स्वयं को पीड़ा पहुँचा कर अथवा किसी अन्य को नष्ट करने के मूर्खतापूर्ण दुराग्रह से जो तप किया जाता है वह तामसिक है।
व्याख्या : पात्र में गन्धक जला कर कुछ लोग अपने सिर पर रखते हैं। कुछ लोग लोहे की कीलें अपने शरीर में चुभोते हैं। अन्य अग्नि को नीचे प्रज्वलित कर के ऊपर अपने शरीर को लटका कर धुंआ कर लेते हैं। कुछ लोग साधना के नाम पर कंठ तक शीत जल में खड़े रहते हैं। अन्य अपने चारों ओर अग्नि जला कर और पाँचवीं अग्नि ऊपर सूर्य की हो, इस प्रकार पञ्चाग्नि तप करते हैं। अन्य अग्नि के घेरे में बैठते हैं। ये तामसिक तप हैं। इनसे आत्म-ज्ञान की प्राप्ति असम्भव है।
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।।२० ।।
शब्दार्थ : दातव्यम् -देना चाहिए, इति-इस प्रकार, यत् -जो, दानम्-दान, दीयते-दिया जाता है, अनुपकारिणे-अनुपकारी को (जिससे प्रत्युपकार की आकाक्षा न हो), देशे स्थान पर, काले-समय पर, च-और, पात्रे सुयोग्य पात्र को, च-और, तत्-वह, दानम् - दान, सात्त्विकम् - सात्त्विक, स्मृतम् -कहा जाता है।
अनुवाद : जो दान अनुपकारी के लिए अर्थात् जिसके प्रति प्रत्युपकार की भावना न रख कर दिया जाये और देश (स्थान), काल (समय) और पात्र को देख कर दिया जाये वह दान सात्त्विक होता है।
व्याख्या : दान उसे देना चाहिए जो बदले में (प्रत्युपकार में) लौटाने में असमर्थ हो अथवा जिससे ऐसे प्रत्युपकार की अपेक्षा न की जाये।
कुरुक्षेत्र हो, वाराणसी हो अथवा संसार में अन्य कोई भी तीर्थ स्थल हो, पावन भूमि हो, वहाँ दान देना उचित है। समय सूर्य ग्रहण अथवा चन्द्र ग्रहण का हो अथवा अन्य कोई भी शुभ काल हो।
पात्रे-शुद्ध अन्तःकरण वाला, तपस्वी जो वेद वेदाङ्ग सहित समस्त शास्त्रों में पारङ्गत हो। जो स्वयं की रक्षा कर सके और दान देने वाले की भी रक्षा करे ।
ऐसे काल और देश में सुयोग्य पात्र दान ग्रहण करने के लिए होना चाहिए जो मानो पवित्रता का अवतार ही हो और सदाचारी हो। ऐसे अत्यन्त गर्व सुयोग्य पात्र को मुक्त हस्त से दान देना श्रेयस्कर है। दान दाता को अपने दान का नहीं होना चाहिए।
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ।।२१ ।।
शब्दार्थ : यत्-जो, तु-वस्तुतः, प्रत्युपकारार्थम् - वापिस लेने के भाव से (यह सोच कर कि कालान्तर में यह मेरा प्रत्युपकार करेगा), फलम् फल, उद्दिश्य-उद्देश्य से, वा-अथवा, पुनः-पुनः, दीयते-दिया जाता है, च-और, परिक्लिष्टम् -क्लेशपूर्वक, तत्-वह, दानम्-दान, राजसम् राजसिक, स्मृतम् माना जाता है।
अनुवाद : वह दान जो प्रत्युपकार की भावना से अथवा किसी उद्देश्य को समक्ष रख कर अथवा क्लेशपूर्वक दिया जाता है वह राजसिक कहा जाता है।
व्याख्या : दान अथवा उपहार जो इस आशा के साथ दिया जाता है कि भविष्य में इसका कुछ प्रतिफल मिलेगा और जन सामान्य में प्रशंसा होगी अथवा इससे अदृश्य स्वर्गिक सुख प्राप्त होंगे, राजसिक कहा जाता है। किसी संन्यासी अथवा ब्राह्मण को भी यदि इस भाव से दान दिया जाये कि इससे पाप-निवृत्ति होगी तो वह भी राजसिक दान है। दान देने के पश्चात् यदि हृदय क्लिष्ट हो तो वह राजसिक दान है।
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ।।२२ ।।
शब्दार्थ : अदेशकाले-अनुचित देश-काल में, यत्-जो, दानम् दान, अपात्रेभ्यः - अयोग्य पात्र को, च-और, दीयते-दिया जाता है, असत्कृतम् -बिना आदर के, अवज्ञातम् -तिरस्कार पूर्वक, तत्-वह, तामसम् - तामसिक, उदाहृतम् -कहा गया है।
अनुवाद : अनुचित स्थान पर, अनुचित काल में, अयोग्य पात्र को बिना सम्मान के तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है वह तामसिक है।
व्याख्या : अदेशकाले-अयुक्त स्थान और काल में। ऐसे स्थान पर जो पावन नहीं है, जहाँ अधर्मी और भिखारी एकत्रित हो जाते हैं, जहाँ अयुक्त साधनों-चोरी, द्यूत आदि से अर्जित धन द्यूत के खिलाड़ियों, गाने वालों, मूर्खी, चोरों और बदनाम औरतों के मध्य विभाजित किया जाता है और ऐसे समय में जो शुभ नहीं है। किन्तु ये आदेश किसी दीन-दुःखी और निर्धन को भिक्षा देने में बाधक नहीं है।
असत्कृतम्-बिना मधुर वाणी के, बिना चरण-प्रक्षालन के अथवा बिना पूजा के, यद्यपि दान समुचित देश-काल में दिया गया है।
दान दाता प्रायः योग्य पात्र मिलने पर भी समुचित श्रद्धा का अभाव रखता है। वह कभी श्रद्धा से शीश नहीं झुकाता। वह पात्र को आसन नहीं प्रदान करता प्रत्युत् उससे तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करता है।
भगवान् कृष्ण अर्जुन से कहते हैं- "मैं बता चुका हूँ कि श्रद्धा, दान, तप, आहार आदि पर निश्चित रूप से तीन गुणों का रङ्ग चढ़ा होता है। निम्न वर्ग का वर्णन करने का मेरा कोई विचार नहीं था किन्तु सर्वोच्च शुचिता को (सत्त्व को) अन्य दो से पृथक् लक्षित करने के लिए मुझे इनका वर्णन करना पड़ा। जब निम्न दो को एक ओर कर दिया जाये तो तीसरा स्पष्ट रूप से श्लाघनीय बन कर, उभर कर आता है जैसे दिन और रात के मध्य संध्या काल । इसी प्रकार रजस् और तमस् का निराकरण किया जाये तो शुद्ध सत्त्व अत्यन्त स्पष्ट हो कर समक्ष आता है और उसकी सर्वाधिक श्रेष्ठ पवित्रता का आभास किया जा सकता है। अतः तुम्हें सात्त्विक प्रकृति प्रत्यक्ष कराने के लिए मैंने अन्य दो का भी वर्णन कर दिया है जिससे तुम उनका त्याग कर के उत्कृष्ट सत्त्व का आश्रय लो और जीवन का लक्ष्य, मोक्ष प्राप्त करो।
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।।२३ ।।
शब्दार्थ : ॐ तत्सत् -ॐ तत्सत्, इति-इस प्रकार, निर्देशः - निर्देश, ब्रह्मणः ब्रह्म का, त्रिविधः-तीन प्रकार का, स्मृतः-कहा गया है, ब्राह्मणाः - ब्राह्मण, तेन-उसके द्वारा, वेदाः- वेद, च-और, यज्ञाः यज्ञ, च-और, विहिताः- कहे गये, पुरा-प्राचीन काल में।
अनुवाद : "ॐ तत् सत्", यह तीन प्रकार का निर्देश अथवा नाम ब्रह्म के लिए कहा गया है। सृष्टि के पूर्व काल में उसके द्वारा ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञों का विधान किया गया।
व्याख्या : 'ॐ तत्सत्' सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का मूल है। ॐ अक्षर ब्रह्म है। तत् वह, अनिर्वचनीय, सत्-ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप ।
परब्रह्म जो समस्त चराचर जगत् का आश्रय है, नाम और रूप-जाति से परे है, वेदों ने उसे नाम देने का साहस किया है। नवजात शिशु का कोई नाम नहीं होता किन्तु नाम मिलने पर वह उत्तर देता है। इस संसार के कष्टों से दुःखी हो कर मनुष्य परम देव से आश्रय का आह्वान करते हैं। ब्रह्म को जब नाम से पुकारा जाये तो वह निराकार होते हुए भी साधक के समक्ष अभिव्यक्त होता है।
इन तीन शब्दों में अपनी ही दिव्य शक्ति निहित है। इनके उच्चारण से उत्पन्न होने वाली तरङ्गे, स्फुरण, कम्पन, मनुष्य की सुप्त दिव्यता को जाग्रत करती हैं और उस परम पुरुष का, जिसका आह्वान किया जा रहा है, आवश्यक प्रतिवचन (उत्तर) भी प्राप्त कराती हैं।
यदि कोई यज्ञादि अनुष्ठान में दोष हो जाये तो इस शक्तिशाली मन्त्रोच्चारण से उस दोष को दूर किया जाता है। इसमें अन्त में 'ॐ तत् सत्' का उच्चारण अथवा इनमें से किसी एक का उच्चारण पर्याप्त है। ॐ अथवाॐॐ तत्सत् के उच्चारण से सभी धार्मिक कृत्य, शास्त्रों का अध्ययन, आध्यात्मिक अनुशासन और ध्यानाभ्यास प्रारम्भ होते हैं। इनमें से किसी एक मन्त्र का जप करने से यजमान सफलता के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को पार कर लेता है।
वेदान्त में ब्रह्मज्ञानियों ने 'ॐ तत् सत्' यह त्रिविध नाम ब्रह्म को दिया है। सृष्टिकर्ता की सृष्टि रचने की शक्ति इसी से निःसृत होती है। उस (परमात्मा) ने जब इस मन्त्र के अर्थ का ध्यान किया और इसका त्रिविध उच्चारण किया तो उसने सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्राप्त की। तब सृष्टिकर्त्ता ने ब्राह्मणों का सृजन किया उनके पथ प्रदर्शन के लिए उन्हें वेदों का ज्ञान दिया तथा यज्ञादि कर्म करने के निर्देश दिये।
पुरा-पूर्व काल में। सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजापति के द्वारा।
ब्रह्मन् शब्द यहाँ वेद का वाचक है।
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ।।२४ ।।
शब्दार्थ : तस्मात् - इसलिए, ॐ-ॐ, इति-इस प्रकार, उदाहृत्य- उच्चारण करके, यज्ञदानतपःक्रियाः- यज्ञ, दान और तप की क्रियायें, प्रवर्तन्ते-प्रारम्भ होती हैं, विधानोक्ताः-शास्त्रों के आदेशानुसार, सततम् -सदा, ब्रह्मवादिनाम् वेद मन्त्रों का उच्चारण करने वालों की।
अनुवाद : इसलिए शास्त्रविहित यज्ञ, दान, तप आदि क्रियायें ब्रह्मवादियों द्वारा सदा “ॐ" के उच्चारण के साथ प्रारम्भ होती हैं।
व्याख्या : शास्त्रवेत्ताओं के मन में 'ॐ' का विशद (सुस्पष्ट) संस्कार, ध्यान के कारण निहित रहता है और वे शुद्ध भाव से 'ॐ' का अथवा प्रणव का सस्वर उच्चारण करते हैं। फिर ॐ का ध्यान कर के, उच्च स्वर से इसका उच्चारण करते हुए वे यज्ञादि क्रिया करते हैं। जिस प्रकार पर्वतारोहण हेतु एक यष्टि (दंड) अनिवार्य है, हितकर है, नदी पार करने के लिए नाव उपयोगी है उसी प्रकार किसी भी मङ्गल कार्य अथवा यज्ञादि के प्रारम्भ में ॐ का उच्चारण अत्यन्त कल्याणकारी एवं महत्त्वपूर्ण है।
ईश्वर का सायुज्य प्राप्त करने के लिए इन शुभ कर्मों का त्याग अपेक्षित नहीं है। आवश्यकता और अपेक्षा केवल इस बात की है कि पूर्ण रूप से समर्पण के भाव से (ईश्वर को समर्पित कर के) सब शुभकर्म करने चाहिए। यज्ञ, दान और तप आत्म साक्षात्कार में प्रतिबन्धक कदापि नहीं हैं, प्रत्युत् इसके विपरीत इन कर्मों को निःस्वार्थ और निष्काम भाव से करने पर मोक्ष सहज हो जाता है।
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपः क्रियाः ।
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्गिभिः ।।२५ ।।
शब्दार्थ : तत् वह, इति-इस प्रकार, अनभिसंधाय-बिना लक्ष्य के, फलम् -फल, यज्ञतपः क्रियाः- यज्ञ और तप की क्रियायें, दानक्रियाः दान की क्रियायें, च-और, विविधाः-विविध, क्रियन्ते-की जाती हैं, मोक्षकाचिभिः मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों द्वारा।
अनुवाद : मोक्ष के जिज्ञासु साधक फल की आकाङ्क्षा त्याग कर 'तत्' शब्द का उच्चारण करते हुए यज्ञ और तप तथा विविध प्रकार की दान की क्रियायें करते हैं।
दानक्रियाः दान कर्म जैसे भू दान, स्वर्ण दान, अन्न दान, वस्त्र दान आदि ।
व्याख्या : तत् -“तत्" शब्द के उच्चारण के साथ।
फलम् -फल । यज्ञ, तप और दान का फल ।
शाश्वत आत्मा जो समस्त ब्रह्माण्ड का अतिक्रमण कर के स्थित है, जो त्रिगुणातीत है, तीन शरीरों, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति की तीन अवस्थाओं से परे है, सब को प्रभासित करने वाला है, सब का आधार है, सब का मूल तत्त्व है, इसी 'तत्' शब्द से अभिहित है। तत् ही उसका सूचक नाम है। ज्ञानी और साधक 'तत्' पर ध्यान करते हैं। वे तत् का उच्चारण कर के कहते हैं-"हमारे समस्त कर्म और कर्मफल 'तत्' (ब्रह्म) को समर्पित हों।
इस प्रकार वे अपने कर्म और कर्मफल ब्रह्म को समर्पित कर के त्याग' का अभ्यास करते हैं। वे अहंभाव और कर्म बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। निष्काम, निरुद्देश्य, निःस्वार्थ कर्म के द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि कर के वे आत्म-ज्ञान प्राप्त करते हैं।
जो कर्म ॐ के उच्चारण से प्रारम्भ कर के शुद्ध और श्रेष्ठ किया जाता है और 'तत्' को समर्पित कर दिया जाता है वह ब्राह्मी प्रकृति में परिवर्तित हो जाता है। “हे अर्जुन, समस्त कर्मों का समापन (विलय) ज्ञान में होता है" (V.33)। यज्ञ-कर्म समझ कर जो कर्म किया जाता है वह अन्ततः ब्रह्म रूप हो जाता है।
तत् शब्द, ऐसे समस्त कर्मों के फल को ईश्वर के लिए समर्पित भाव का सांकेतिक शब्द है। यदि तुम तत् शब्द का उच्चारण करते हो, तो उसका समर्थक भाव यही है-"वे (कर्म, कर्मफल) मेरे नहीं हैं।" ॐ के उच्चारण से जिस कृत्य का प्रारम्भ किया था वह तत् के उच्चारण के साथ ब्रह्म को समर्पित हुआ। अगले श्लोक में सत् शब्द का प्रयोग निरूपित है।
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते ।।२६।।
शब्दार्थ : सद्भावे-वास्तविकता के भाव में, साधुभावे साधुभाव में अर्थात् अच्छाई के भाव में, च-और, सत्-सत्, इति-इस प्रकार, एतत् यह, प्रयुज्यते-प्रयोग किया जाता है, प्रशस्ते-शुभ, कर्मणि-कर्म में, तथा- और, सत् सत्, शब्दः -शब्द, पार्थ- हे पार्थ, युज्यते-प्रयोग होता है।
अनुवाद : सत् शब्द वास्तविकता और भद्रता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हे अर्जुन, शुभ कर्म के भाव में सत् शब्द का प्रयोग होता है।
व्याख्या : सत्-भाव-वह जो परिवर्तनशील के मध्य अपरिवर्तशील है, अनित्य के मध्य नित्य है और जो भूत, भविष्यत् और वर्तमान में विद्यमान है, वह सत् है। नित्य परिवर्तनशील नाम, रूपों में निहित वास्तविकता सत् है। नित्य विकार को प्राप्त होने वाले रूपों का आश्रय सत् है। शुभ, प्रशंसनीय कर्म सत् है।
साधु भाव-प्रकृति के साथ समन्वय का वाच्य, जिससे संसार चक्र निर्बाध चलता रहे।
दोषपूर्ण कर्म को निर्दोष और पूर्ण करने के लिए सत् शब्द अत्यन्त शक्तिशाली है। जब किसी मङ्गल कार्य में कोई त्रुटि रह जाने से 'असत्' की सम्भावना होती है तो 'सत्' शब्द का प्रयोग उसे दोषमुक्त करता है और कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होता है। सत् शब्द कर्म के 'असत् भाव' को दूर कर के इसे पूर्ण करता है क्योंकि इसमें परिमार्जन और पूर्णत्व की शक्ति है।
सत् पर-ब्रह्म है। सत् शाश्वत, स्वयं प्रकाश, अखण्ड, असीम, अनिर्वचनीय, गोपनीय ब्रह्म का वर्णनातीत, अकथ्य लक्षण है।
किसी विषय की वास्तविकता अभिव्यक्त करनी हो जो वस्तुतः, वास्तविक (सत्य) नहीं है अथवा अपेक्षाकृत सत्य है जैसे अविद्यमान पुत्र के जन्म होने में, जो अवास्तविक है किन्तु सापेक्ष भाव में वास्तविक है। किसी मनुष्य को सदाचारी कहना जब कि वह सदाचारी नहीं है अथवा अपेक्षाकृत अच्छा है और यह कहना कि अमुक कृत्य शुभ है जब कि वह शुभ नहीं है अथवा अपेक्षाकृत शुभ है-ऐसे भावों में ब्रह्म के सत् नाम का प्रयोग किया जाता है।
ब्रह्म ही सत्य है। केवल वह सत् है, उसी का अस्तित्व है। किन्तु गोविन्दन के पुत्र उत्पन्न होने पर हम कहते हैं कि गोविन्दन का पुत्र अस्तित्व में आ गया है। ब्रह्म विचार किया जाये तो गोविन्दन का पुत्र तो अस्तित्वमान् है ही नहीं।
सत् शब्द जो ब्रह्म के नाम का वाचक है वह गोविन्दन के पुत्र के लिए भी प्रयोग हो रहा है जो वास्तविक नहीं है अथवा अपेक्षाकृत सत्य है। केवल ब्रह्म ही पूर्णरूप से शुभ और श्रेष्ठ है किन्तु सत् शब्द जो केवल ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होना चाहिए वह कर्म के लिए भी प्रयोग होता है जो पूर्ण रूप से तो शुभ नहीं है किन्तु अपेक्षाकृत शुभ है। सत् का प्रयोग अपूर्ण कर्मों को पूर्णता प्रदान करने के लिए होता है।
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।।२७ ।।
शब्दार्थ : यज्ञेयज्ञ में, तपसि-तप में, दाने-दान में, च-और, स्थितिः-स्थिरता को, सत्-सत्, इति-इस प्रकार, च-और, उच्यते-कहा जाता है, कर्म-कर्म, च-और, एव-ही, तदर्थीयम् - इन के सम्बन्ध में अथवा ब्रह्म के लिए, सत्-सत्, इति-इस प्रकार, एव-ही, अभिधीयते-कहा जाता है।
अनुवादः यज्ञ, तप और दान में स्थिरता सत् कही जाती है और इनसे सम्बद्ध कर्म (अथवा परमात्मा के लिए कर्म) भी सत् कहे जाते हैं।
व्याख्या : यज्ञ, तप, दान और अन्य समस्त कर्म यदि तुम परमात्मा को समर्पित कर के अन्तःकरण की शुद्धता और सत्यता के साथ करते हो तो तुम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य-मोक्ष, शाश्वत आनन्द प्राप्त करोगे । ब्रह्म के लिए और ब्रह्म के नाम पर यदि तुम कर्म करते हो तो तुम पर परमात्मा की परम शान्ति और पूर्णत्व की वृष्टि होगी।
यदि तुम अपनी श्रद्धा 'ॐ' अथवा 'ॐ तत्सत्' में एकाग्र करते हो तो तुम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओगे। कोई भी यज्ञ, तप अथवा दान क्रिया और कर्म यदि तुम निःस्वार्थ भाव से और निष्काम भाव से प्रभु को कर्म और कर्मफल सहित समर्पित करते हुए श्रद्धा, भाव और भक्ति से 'सत्' का उच्चारण करते हुए करते हो तो तुम्हें कर्म में सिद्धि और सफलता प्राप्त होगी।
अपूर्ण और असात्त्विक यज्ञ कर्म, तप, दान आदि की क्रियायें भी पूर्ण और सात्त्विक हो जायेंगी।
तदर्थीयम् - तत्+अर्थ+इयम्-अर्थात् यज्ञ, तप और दान ।
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ।।२८ ।।
शब्दार्थ : अश्रद्धया-बिना श्रद्धा के, हुतम् - किया हुआ हवन, दत्तम् -दिया हुआ दान, तपः-तप, तप्तम् - किया हुआ (तप), कृतम् -किया हुआ कर्म, च-और, यत्-जो भी, असत् -असत् . इति-इस प्रकार, उच्यते-कहा जाता है, पार्थ-हे पार्थ, न-नहीं, च-और, तत्-वह, प्रेत्य-मरने के बाद,न -नहीं , इह-इस लोक में।
अनुवाद : बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और किया हुआ तप 'असत्' कहलाते हैं इसलिए हे अर्जुन, ये न तो इस लोक में न ही मरणोपरान्त फल देने वाले हैं।
व्याख्या : असत्-जिसका रूप बदलता रहता है, स्थिर अस्तित्व नहीं है। यहाँ इसका अभिप्राय यह नहीं कि जिसका असि हो।
जो भी कृत्य यज्ञ, तप और दान बिना श्रद्धा अथवा किसी दबाव में अथवा किसी प्रकार की विपत्ति को टालने अथवा किसी वासना की पूर्ति हेतु किये जाते हैं, वे असत् प्रकृति के हैं। वे किसी को स्थिर परिणाम नहीं दे सकते।
परमात्मा को समर्पित किये बिना यज्ञ, तप और दान क्रिया अनुष्ठान कर्ता को इहलोक अथवा परलोक में कोई फल देने वाली नहीं होगी। ये क्रियायें उतनी ही व्यर्थ होंगी जितनी कि पर्वतीय प्रदेश में चट्टानों पर गिरती वर्षा की बूँदें अथवा भस्मीभूत अग्नि में डाली गई घृत आहुतियाँ। बिना श्रद्धा के मनुष्य अहंकारी और दम्भी बन जाता है। उसका हृदय कठोर हो जाता है। बिना श्रद्धा के शत-शत यज्ञ भी क्यों न किये जायें और ईश्वर को समर्पण भाव से क्यों न हों समस्त विश्व की सम्पदा भी यदि बिना श्रद्धा और समर्पण भाव के दान कर दी जाये, इसका कोई मूल्य नहीं होगा। यह व्यर्थ होगा। ज्ञानी जन इस प्रकार के यज्ञ और दान की स्तुति नहीं करेंगे। शक्ति, धन और समय का ही व्यर्थ में नाश होगा ।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ।।१७ ।।
।। इति श्रद्धात्रयविभागयोगः ।।
ॐ श्री परमात्मने नमः
अथाष्टादशोऽध्यायः
मोक्षसंन्यासयोगः
अर्जुन उवाच
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ।।१ ।।
शब्दार्थ : संन्यासस्य-संन्यास का, महाबाहो - हे महाबाहो, तत्त्वम् तत्त्व को, इच्छामि इच्छा करता हूँ, वेदितुम् - जानने की, त्यागस्य-त्याग की, च-और, हृषीकेश- हे कृष्ण, पृथक् पृथक् रूप से, केशिनिषूदन- हे केशि को मारने वाले ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे महाबाहो! हे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन ! मैं संन्यास का और त्याग का यथार्थ अभिप्राय पृथक् पृथक् जानना चाहता हूँ।
व्याख्या : इस प्रवचन में सम्पूर्ण गीता का सार अत्यन्त सुन्दर रूप में परिलक्षित किया गया है। इस अन्तिम प्रवचन अथवा आदेश में पूर्व अध्यायों में दिये गये ज्ञान का अप्रतिम सार दिया गया है। अर्जुन संन्यास और त्याग के भेद को जानने का इच्छुक है।
केशि एक असुर था जिसका भगवान् कृष्ण ने संहार किया था इसलिए अर्जुन उन्हें केशिनिषूदन कह कर संबोधित कर रहे हैं।
पूर्व अध्यायों में संन्यास और त्याग शब्दों का प्रयोग इतस्ततः हुआ है किन्तु उनके अर्थों पर पृथक्तया प्रकाश नहीं डाला गया। इसलिए अगले श्लोक में भगवान् कृष्ण दोनों शब्दों के अर्थ स्पष्ट करते हैं।
श्री भगवानुवाच
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ।।२ ।।
शब्दार्थ : काम्यानाम् - इच्छित, कर्मणाम् -कर्मों का, न्यासम् - त्याग, संन्यासम् -संन्यास, कवयः- ज्ञानी, विदुः-समझते हैं, सर्वकर्मफलत्यागम् - सब कमाँ के फल का त्याग, प्राहुः-कहते हैं, त्यागम्-त्याग, विचक्षणाः बुद्धिमान् ।
श्री भगवान् ने कहा
अनुवाद : इच्छित कर्मों के न्यास को ज्ञानी जन संन्यास कहते हैं, अन्य बुद्धिमान् पंडितजन समस्त कर्मों के फल के त्याग को 'त्याग' कहते हैं।
व्याख्या : काम्य कर्माणि - अश्वमेध यज्ञ आदि विशेष अनुष्ठान और क्रियायें जो विशेष लक्ष्यै की प्राप्ति हेतु किये जाते हैं। बुद्धिमान् लोग कहते हैं कि सभी नित्य और नैमित्तिक कर्मों के फल के त्याग का अभिप्राय 'त्याग' है।
संन्यास और त्याग शब्द का मूल अर्थ है छोड़ देना (त्याग देना) । सामान्य भाव में ये दोनों शब्द पर्यायवाची माने जाते हैं। दोनों का अर्थ 'त्याग' है। इन दोनों का अर्थ फल और पत्थर अथवा पात्र और वस्त्र की भाँति सर्वथा पृथक् नहीं है। अत्यल्प भेद से दोनों एक ही भाव को स्पष्ट करते हैं।
एक आलोचक का कथन है- नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल नहीं होता। तो फिर उनके फल त्याग का प्रश्न ही कहाँ उठता है? यह तो वन्ध्या के पुत्र त्याग की भाँति हुआ!
हमारे विचार से यह तर्क उचित नहीं है। भगवान् कहते हैं नित्य और नैमित्तिक कर्मों का भी फल होता है (XVIII.12) । केवल संन्यासी, जिन्होंने कर्मफल का त्याग कर दिया है वे फल प्राप्ति नहीं करेंगे किन्तु अन्य लोग तो नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल प्राप्त करेंगे।
आत्म साक्षात्कार के उपरान्त यदि समस्त कर्मों का त्याग कर के कोई जीवन के चतुर्थ आश्रम-संन्यास में प्रवेश पाता है तो यह विद्वत्-संन्यास कहलाता है। यदि कर्मों का त्याग कर के कोई पुरुष वेदान्त विचार अथवा वेदान्त दर्शन के सत्य का विश्लेषण आत्मा-परमात्मा का सायुज्य कराने वाले उपनिषदों के महावाक्य पर विचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करता है और इस विधि के संन्यास से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है तो इसे विविदिशा संन्यास कहा जाता है।
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ।। ३ ।।
शब्दार्थ : त्याज्यम् -त्यागने योग्य, दोषवत्-दोष की भाँति, इति-इस प्रकार, एके कुछ, कर्म कर्म, प्राहुः कहते हैं, मनीषिणः-विद्वान, यज्ञदानतपःकर्म-यज्ञ, दान और तप के कर्म, न-नहीं, त्याज्यम् त्यागने चाहिए, इति-इस प्रकार, च-और, अपरे अन्य ।
अनुवाद : कुछ विद्वानों का मत है कि दोष समझ कर कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। अन्य पंडितजन कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप आदि कमाँ का त्याग नहीं करना चाहिए।
व्याख्या : कुछ सांख्य मतावलम्बी दर्शनकार ऐसा सोचते हैं कि समस्त कर्म (शुभाशुभ) दोषवत् त्याज्य हैं।
दोषवत् बुराई मान कर। सभी कर्म त्याज्य हैं क्योंकि वे दोषयुक्त हैं, वे बन्धन का कारण हैं अथवा उन्हें रजोगुण से युक्त अथवा अन्य अशुभ वृत्तियों से युक्त मान कर त्याग देना चाहिए।
अन्य दार्शनिकों का यह मत है कि यज्ञ, दान और तप कर्म का त्याग, कर्मयोग के योग्य लोगों को नहीं करना चाहिए।
अब सुनो, मैं इस समस्या का समाधान करूँगा और बताऊँगा कि त्याग का अभ्यास कैसे करना है।
यहाँ केवल कर्मयोगियों के विषय में चर्चा हो रही है, उन योगियों के विषय में नहीं, जो इस पथ से ऊपर (परे) पहुँच चुके हैं। ये विरोधी विचारधारायें कर्मयोगियों के विषय में चल रही हैं। सांसारिकता से अतीत ज्ञानी और संन्यासीवृन्द के लिए यह चर्चा नहीं है।
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ।।४ ।।
शब्दार्थ : निश्चयम् - निश्चय (अन्तिम सत्य), शृणु सुनो, मे—मेरा, तत्र-वहाँ, त्यागे-त्याग के विषय में, भरतसत्तम- हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, त्याग -त्याग, हि-निश्चित रूप से, पुरुषव्याघ्र- हे पुरुष श्रेष्ठ (पुरुषसिंह), त्रिविधः-तीन प्रकार का, संप्रकीर्तितः- कहा गया है।
अनुवाद : हे भरत श्रेष्ठ! हे पुरुष श्रेष्ठ ! अब त्याग के विषय में मुझ से सुनो। निश्चित रूप से त्याग तीन प्रकार का कहा गया है।
व्याख्या : अब भगवान् अपना निर्णायक मत देते हैं। शास्त्रों में निर्दिष्ट है कि त्याग तीन प्रकार का होता है-सात्त्विक, राजसिक और तामसिक । केवल भगवान् ही इस विषय की यथार्थता पर अन्तिम प्रकाश डाल सकते हैं। इस संसार के दुःखों से मुक्त होने के सभी इच्छुक साधकों को त्याग की वास्तविक प्रकृति को समझना चाहिए।
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।।५ ।।
शब्दार्थ : यज्ञदानतपःकर्म-यज्ञ, दान और तप के कर्म, न - नहीं, त्याज्यम् - त्यागने चाहिए, कार्यमेव-करने ही चाहिए, तत्-वह, यज्ञः यज्ञ, दानम् दान, तपः-तप, च-और, एव-ही, पावनानि-पावन, मनीषिणाम् - विद्वानों के।
अनुवाद : यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए। ये कर्म करने योग्य हैं। यज्ञ, दान और तप कर्म बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं।
व्याख्या : फल की आकाङ्क्षा से शून्य हृदय वाले विद्वत्वृन्द के लिए यज्ञ, दान और तप कर्म पवित्र करने वाले हैं, उनके अन्तःकरण की शुद्धि करने वाले हैं। ये कृत्य कर्म अवश्य करने चाहिए। कुशलतापूर्वक किये गये कर्म बन्धन में डालने की शक्ति खो देते हैं और आत्मा को भौतिक बन्धनों से मुक्त करने वाले होते हैं।
अब हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह कौशल बताऊँगा जिससे कर्म अपना प्रभाव स्वयं नष्ट कर देते हैं।
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ।।६ ।।
शब्दार्थ : एतानि-ये, अपि-भी, तु-किन्तु, कर्माणि-कर्म, सङ्गम् - आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग कर, फलानि -फल, च-और, कर्तव्यानि करने योग्य हैं, इति इस प्रकार, मे मेरा, पार्थ- हे अर्जुन, निश्चितम् -निश्चित, मतम् -मत, उत्तमम् -उत्तम ।
अनुवाद : किन्तु हे अर्जुन, फल की इच्छा त्याग कर और आसक्ति को भी त्याग कर ये कर्म किये जाने चाहिए। यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है।
व्याख्या : यह कर्म योग के सिद्धान्त का सार है जिसका वर्णन पूर्वतः अनेक श्लोकों में आ चुका है। दोष कर्म में नहीं होता प्रत्युत् फल की कामना और आसक्ति में होता है।
एतानि अपि-ये भी। यज्ञ, दान और तप भी। अन्य निष्काम कर्मों की भाँति । एतान्यपि, अन्य कर्मों के साथ यज्ञ, दान और तप कर्मों को लक्ष्य कर के कहा गया है। जो कर्म निष्काम भाव से आसक्ति को त्याग कर कर्तव्य कर्म मान कर किये जाते हैं वे मोक्ष में बाधक नहीं होते । फल की आशा त्याग कर किये गये कर्मों का रजस् और तमस् नष्ट हो जाता है और वे सत्त्व से पूरित हो जाते हैं। निष्काम भाव से विवेकपूर्ण किये गये कर्म, कर्म बन्धन की श्रृंखला (कारण और कार्य रूप) को नष्ट करने में सहायक होते हैं।
भगवान् ने कहा- "मुझसे त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो" (श्लोक ४)! तब पूर्ण अधिकार के साथ भगवान् ने कहा कि यज्ञ, दान और तप कमाँ का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि वे बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं। "ये कर्म भी करने चाहिए", ये मात्र, भगवान् का श्लोक ४ में उपदिष्ट अन्तिम निर्णय है।
'अपि' शब्द का अर्थ है कि यज्ञ, दान, तप कर्म यद्यपि आसक्ति से युक्त और फल की आकाङ्क्षा करने वाले साधक को बन्धन में डालने वाले हैं तदपि करने योग्य हैं।
जिस प्रकार वृक्ष के बीज भस्मीभूत कर के व्यर्थ कर दिये जाते हैं उसी प्रकार साधक फल की इच्छा त्याग कर कर्म की फल प्रदान करने की शक्ति को जला देता है।
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ।।७ ।।
शब्दार्थ : नियतस्य-नित्य (कर्म) का, तु-किन्तु, संन्यासः-त्याग, कर्मणः कर्म का, न - नहीं, उपपद्यते-उचित है, मोहात्-मोह वश, तस्य- उसका, परित्यागः-त्याग, तामसः-तामसिक, परिकीर्तितः-कहा गया है।
अनुवाद : निश्चित रूप से नित्य कर्मों का त्याग उचित नहीं है। शास्त्र विहित नित्य कर्मों का मोह वश त्याग तामसिक कहा गया है।
व्याख्या : विहित कर्मों का त्याग उचित नहीं है क्योंकि यह अज्ञानी मनुष्यों के लिए शुद्धि के हेतु माने गये हैं। नियत कर्म तो अवश्य करने योग्य कर्तव्य कर्म होते हैं, उनका त्याग कैसे हो सकता है? केवल तमस् की प्रधानता में मोह वश ही ऐसा हो सकता है। नियत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वह मोहान्धकार में पड़ा है, अज्ञान में है। तमस् ही अज्ञान है।
नियत-स्व धर्मानुसार नियत कर्म। नियत कर्म तो अवश्य किये जाने योग्य कर्तव्य कर्म को कहते हैं। उसका त्याग तो आत्म-विरुद्ध सत्य हो जाता है।
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ।।८ ।।
शब्दार्थ : दुःखम् दुःखद, इति-इस प्रकार, एव-ही, यत्-जो, कर्म-कर्म, कायक्लेशभयात् - शारीरिक क्लेश के भय से, त्यजेत्-त्याग दे, सः-वह, कृत्वा कर के, राजसम् - राजस्, त्यागम्-त्याग, न-नहीं, एव-ही, त्यागफलम् त्याग के फल को, लभेत्-प्राप्त करता है।
अनुवाद : शारीरिक दुःख के भय से (क्योंकि यह दुःखद है), कर्म का त्याग करने वाला त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता क्योंकि यह राजसिक त्याग है।
व्याख्या : फलम् -फल, अनुदान । मोक्ष अथवा आत्मसाक्षात्कार, जो विवेकपूर्ण किये गये कर्मों के फल के त्याग का प्रतिफल (परिणाम) है।
शास्त्र विहित कर्म और धार्मिक कृत्य करने के लिए दृढ़ संकल्प और सतत् एकाग्र चित्तप्रवृत्ति की आवश्यकता होती है।
सम्भव है कोई व्यक्ति इसे प्रारम्भ तो करे किन्तु शारीरिक अथवा किसी अन्य कष्ट के कारण इसे मध्य में ही त्याग दे।
तो सात्त्विक त्याग क्या है? भगवान् कहते हैं-
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ।।९ ।।
शब्दार्थ : कार्यम् -कर्तव्य कर्म, इति-इस प्रकार, एव-ही, यत्-जो, कर्म-कर्म, नियतम् -नित्य कर्म, क्रियते-किया जाता है, अर्जुन-हे अर्जुन, सङ्गम् आसक्ति, त्यक्त्त्वा-त्याग कर, फलम्-फल, चऔर, एव-ही, सः- वह, त्यागः-त्याग, सात्त्विकः-सात्त्विक, मतः- माना जाता है।
अनुवाद : हे अर्जुन! जो भी नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा त्याग कर केवल इसलिए किया जाता है कि वह करना धर्म है अथवा कर्तव्य है, वह कर्म सात्त्विक माना जाता है।
व्याख्या : सात्त्विक प्रकृति का मनुष्य अपने भाग्य से प्राप्त कमाँ को करता है जो उसे दैवात् उसकी योग्यता और सहज प्रकृति के अनुरूप मिलते हैं। न तो उसे अपने कर्मों का अभिमान होता है न ही उन कर्मों के फल की आशा होती है।
अज्ञानी व्यक्ति के मन में यह भाव उदित हो सकता है कि नित्य कर्म आत्म-शुद्धि अथवा पाप निवृत्ति का फल अनुष्ठानकर्त्ता को प्रदान कर रहे हैं किन्तु इस प्रकार की आशा अथवा फल की इच्छा का भी त्याग करना अनिवार्य है। इस श्लोक में कर्म-फल-इच्छा के परित्याग की स्तुति की गई है।
कर्तृत्व भाव को त्याग कर निःस्वार्थ और निष्काम भाव से जब मनुष्य अपने नित्य कर्म करता है तो उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, दिव्य ज्योति को प्राप्त करने के लिए वह तैयार हो जाता है और आत्म-ज्ञान का अभ्युदय होता है। वह ज्ञान-निष्ठ हो जाता है।
मुमुक्षु साधक को कायिक क्लेश सहन करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। आत्म-अनुशासन अथवा परित्याग के समस्त कर्म शारीरिक कष्टों से जुड़े होते हैं।
पुनः यही गीता का सार है-
आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करें।
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।।१० ।।
शब्दार्थ : न - नहीं , द्वेष्टि-द्वेष करता है, अकुशलम् -प्रतिकूल, अप्रिय को, कर्म-कर्म, कुशले अनुकूल, प्रिय, न-नहीं, अनुषज्जते-लिप्त होता है, त्यागी-त्यागी, सत्त्वसमाविष्टः-सत्त्व से युक्त, मेधावी-बुद्धिमान्, छिन्नसंशयः जिसके संशय नष्ट हो गये हों।
अनुवाद : वह त्यागी मनुष्य जो सात्त्विक है, मेधावी है और जिसके संशय नष्ट हो चुके हैं, अप्रिय कर्म के प्रति घृणा भाव नहीं रखता और प्रिय कर्म से अनुराग नहीं करता ।
व्याख्या : त्यागी मनुष्य सब कर्मों का समान रूप से स्वागत करता है। वह सुख-दुःख से प्रभावित नहीं होता। रुचिकर कर्म करने में वह हर्षित नहीं होता और अप्रिय कर्म करने पर दुःखी नहीं होता। न तो उसे पूर्व कर्म में आसक्ति है न पश्चात् कर्म में द्वेष भाव है। प्रिय के प्रति उसमें आकषर्ण नहीं और अप्रिय के प्रति विकर्षण नहीं। किसी भी कर्म अथवा कर्म फल में विरक्त होने के कारण वह लोक कल्याण के लिए कर्म रत होगा।
अकुशलम् कर्म-अप्रिय कर्म अथवा फल की इच्छा से कर्म करना, जो संसार में बन्धन का कारण है क्योंकि पुनः शुभाशुभ कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। किन्तु त्यागी तो सोचेगा "यह कर्म किस उपयोग का?" और वह अप्रिय कर्म से घृणा नहीं करेगा।
कुशले-प्रिय कर्म जिनमें नित्य कर्म भी सम्मिलित हैं। यह सोच कर भी, कि ये कर्म मोक्ष दिलाने वाले हैं, वह इनसे प्रेम नहीं करता।
कर्म के प्रति आसक्ति और कर्म फल की इच्छा त्याग कर पूर्ण शक्ति से निष्काम कर्म करने वाले साधक का अन्तःकरण सत्त्व से पूर्ण हो कर उसमें सत्य और असत्य तथा नित्य और अनित्य का विवेक जाग्रत करता है। तब उसमें ज्ञान का सूर्योदय होता है जो अज्ञानान्धकार से उत्पन्न समस्त संशयों का विनाश कर देता है। अब उसे ज्ञान होता है कि परमानन्द, शाश्वत शान्ति और अमृतत्व की प्राप्ति हेतु आत्म-ज्ञान ही हेतुक है। अब उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं। संशय की प्रकृति क्या है? "ब्रह्म का अस्तित्व है अथवा नहीं?" उपनिषदों में सगुण ब्रह्म की चर्चा है अथवा निर्गुण ब्रह्म की? व्यष्टि आत्मा (जीवात्मा) समष्टि आत्मा (परमात्मा) से एक रूप है अथवा नहीं? मुझे आत्म-ज्ञान होगा अथवा नहीं? प्रारब्ध, संचित अथवा आगम-इनमें से किसी का मुझ पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं? यह संसार, जिसकी प्रकृति इस भाव की है कि 'मैं कर्ता हूँ', 'मैं भोक्ता हूँ', मन से सम्बद्ध है, बुद्धि से अथवा आत्मा से ? मोक्ष के साधन कौन-कौन से हैं-योग, भक्ति, कर्म अथवा आत्म-ज्ञान? क्या आत्म- साक्षात्कार सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य अवस्थाओं का स्वरूप है?
कर्म योग करने पर मनुष्य का हृदय परिमार्जित होता है। हृदय की शुद्धता से वह स्वयं को निर्विकार, निष्क्रिय आत्म तत्त्व समझने लगता है जो अजन्मा है, न स्वयं कर्ता है और न करवाता ( V .13) । उसे कर्म से मुक्ति और आत्म-ज्ञान के प्रति भक्ति की भावना प्राप्त होती है। इस श्लोक में ऊपर कहे गये कर्म योग का उपदेश दिया गया है।
मेधावी बुद्धि से युक्त। स्थितप्रज्ञ । फिर 'मेधा' क्या है? 'अहं ब्रह्मास्मि' अथवा 'तत्त्वमसि' महा-वाक्यों का यथार्थ ज्ञान और उन पर किये गये अनन्यमनस्क ध्यान द्वारा प्राप्त जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का सद्यः ज्ञान जो तीन प्रकार के संशय-संशय भावना (doubt), असम्भावना (improbability) और विपरीत भावना (perversion) से मुक्त है और पुरुषार्थ चतुष्टय (अध्याय III.3) के अभ्यास और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा और सत्य-ज्ञान के श्रवण से प्राप्त होती है।
ऐसा मेधावी पुरुष यह नहीं सोचेगा कि निषिद्ध कर्म जो अज्ञानी को बन्धन में डालने वाले हैं, उसे भी प्रभावित करेंगे अथवा उसके प्रतिकूल होंगे। वह यह नहीं सोचेगा कि यदि उसे वे कर्म करने पड़ेंगे तो वह भी बन्धन में आ जायेगा क्योंकि वह अच्छे-बुरे, गुण-अवगुण, सत्य-असत्य से परे पहुँच चुका है। अब उसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। वह तो यह भाव रखता है कि वह अब कृतकृत्य है अर्थात् उसने समस्त कर्म समाप्त कर लिए हैं।
इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि वह अब अनुचित कर्म करेगा । क्योंकि उसकी इच्छा अब परमात्मा की इच्छा हो चुकी है, वैश्विक हो चुकी है, वह शास्त्र विहित कर्म ही करेगा। वह णास्त्र के नियमों के विरुद्ध कदापि नहीं जायेगा। परमात्मा ही उसकी इन्द्रियों और मन के द्वारा कार्य करते हैं क्योंकि उसकी व्यक्तिगत इच्छा तो अब है ही नहीं।
राग-द्वेष मनुष्य को संसार की ओर प्रेरित करने वाली वृत्तियाँ हैं। मेधावी पुरुष और संन्यासी में इन वृत्तियों का अभाव होता है अतः वे कर्म अथवा कर्म फल त्यागने में शक्य होते हैं।
क्षुब्धार्णव (stormy ocean) जिस प्रकार शान्त रहता है अर्थात् प्रचंडवात और लहरों के उठने पर भी सागर अपनी सीमा का उल्लंघन (व्यतिरेक) नहीं करता, शान्त रहता है उसी प्रकार सात्त्विक मनुष्य जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी शान्त रहता है। वह जान लेता है कि जीवन की (दैव वशात्) घटनायें अनिवार्य अथवा अपरिहार्य हैं। वह विभिन्न प्रकार से क्रिया करेगा किन्तु समन्वित और स्थिरचित्त होने के कारण क्षुब्ध नहीं होगा।
कर्तव्य कर्म यदि अरुचिकर परिणाम देने वाला भी हो, खतरा अथवा दुर्भाग्यपूर्ण फल दे रहा हो, शारीरिक कष्ट देने वाला हो, अप्रिय हो, प्रतिकूल हो तो भी उसके प्रति घृणा का भाव मन में नहीं लाना चाहिए। ऐसा कर्म भी सहृदय स्वीकार कर के पूर्ण संलग्नता से करना चाहिए। इसका प्रयोजन और इसकी अनिवार्यता के विषय में तुम्हें यथार्थ और पूर्ण समझ होनी चाहिए। भगवान् द्वारा प्रदत्त कर्म करने की आवश्यकता और महत्त्व को समझने में अर्जुन प्रारम्भ में असफल रहा। वह अपना मूर्खता पूर्ण दर्शन समझाने लगा। नियत कर्म को वह करने में सफल न हो सका क्योंकि अज्ञानवश उसने सोचा कि लोगों का संहार करना शुभ कर्म नहीं था किन्तु अन्त में जब भगवान् के अमोघ उपदेश से उसके नेत्र खुले तो वह कर्म की आवश्यकता और उसके अभिप्राय को जान गया यद्यपि वही कर्म उसे अप्रिय लग रहा था। वह बोला- "मेरा मोह नष्ट हो गया है। हे कृष्ण, आपकी अहेतुकी कृपा से मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैं कृत संकल्प हूँ। मेरे संशय समाप्त हो गये हैं। मैं आपके उपदेश का अनुसरण करूँगा।"
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।। ११ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, हि-वस्तुतः, देहभृता-देहधारी के द्वारा, शक्यम् -सम्भव, त्यक्तुम् -त्याग करना, कर्माणि-कर्म, अशेषतः- पूर्णरूपेण, यः-जो, तु-किन्तु, कर्मफलत्यागी-कर्म फल का त्याग करने वाला, सः- यह, त्यागी-त्यागी, इति-इस प्रकार, अभिधीयते-कहा जाता है।
अनुवाद : निश्चित रूप से, किसी देहधारी के लिए पूर्णरूपेण कर्मों का त्याग सम्भव नहीं है किन्तु जो कर्म फल का त्याग करता है वह वस्तुतः त्यागी है।
व्याख्या : देह धारण कर के भी कर्म करने में जो व्यक्ति खेद का अनुभव करता है वह वास्तव में मूर्ख है। उष्णता के स्वाभाविक गुण से युक्त अग्नि क्या अपने गुण से छुटकारा प्राप्त कर सकता है? जब तक तुम इस देह को धारण किये हो, कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान् कृष्ण अर्जुन से कहते हैं- 'कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अकर्मकृत् नहीं हो सकता क्योंकि स्वाभाविक गुणों से आकृष्ट हो कर वह स्वयं ही कर्म करने के लिए गुणों द्वारा वशीभूत हो कर (कर्म करने को) बाध्य हो जाता है।' (III.5) प्रकृति और तुम्हारा अपना स्वभाव भी तुम्हें कर्म के लिए प्रेरित करेंगे। तुम्हें कर्तृत्वभाव और कर्म फल की आकाङ्क्षा का त्याग करना होगा। केवल तभी तुम सुरक्षित हो, कोई कर्म तुम्हें बन्धन में नहीं डालेगा।
अज्ञानी मनुष्य जो देह में आत्मा का अध्यास करता है और सोचता है कि वही कर्ता है, ऐसे व्यक्ति को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उसके लिए कर्म त्याग करना असम्भव है। फल की आशा त्यागने के लिए उसे समस्त शास्त्र विहित कर्म करने होंगे।
देहभृत्-देह को धारण करने वाला। आत्माभिमान रखने वाला अथवा शरीर को आत्मा के साथ एकरूप (तादात्म्य रूप) मानने वाला देहभृत् है। सत्य-असत्य, शाश्वत और क्षणभङ्गुर के भेद को जानने वाला विवेकी पुरुष देहभृत् नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह स्वयं को कर्ताभाव से पृथक् मानता है (II.21), जो मनुष्य, हे अर्जुन, उसे जानता है जो अविनाशी है, शाश्वत है, अजन्मा है, अक्षय्य है-वह किसी को कैसे मार सकता है अथवा मरवा सकता है?
तत्त्व ज्ञान से शून्य व्यक्ति जब कर्म फल की इच्छा का त्याग कर के नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता है तो कर्म करते हुए भी त्यागी कहलाता है। स्तुति के अभिप्राय से उसे यह उपाधि दी जाती है।
केवल तत्त्व ज्ञानी के लिए ही समस्त कर्मों का त्याग सम्भव है क्योंकि बह देहातीत हो चुका है अब वह देहभृत् नहीं है। (निरूपण - 111.5)
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ।।१२ ।।
शब्दार्थ : अनिष्टम् अप्रिय, अशुभ, प्रतिकूल, इष्टम् -प्रिय, शुभ, अनुकूल, मिश्रम् -मिश्र, च-और, त्रिविधम्-तीन प्रकार का, कर्मणः कर्म का, फलम् - फल, भवति होता है, अत्यागिनाम्-त्याग न करने वालों का, प्रेत्य-मृत्यूपरान्त, न नहीं, तु-किन्तु, संन्यासिनाम् -संन्यासियों का, क्वचित् -कोई।
अनुवाद : अत्यागियों (कर्मनिष्ठ अज्ञानियों) को मृत्यूपरान्त तीन प्रकार के फल-प्रिय, अप्रिय और मिश्र मिलते हैं किन्तु ज्ञान निष्ठ संन्यासियों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता।
व्याख्या : कोई तो कर्म फल प्रिय है, कोई अप्रिय और अन्य मिश्र हैं। जिनमें शुभ कर्मों का अतिरेक होता है वे देव रूप में जन्म लेते हैं। अशुभ कर्म करने वाले पशु जगत् अथवा वनस्पति जगत् में पुनर्जन्म लेते हैं। यदि उनके शुभाशुभ कर्म समान हैं तो वे मनुष्य योनि में आते हैं। ये शुभ, अशुभ और मिश्र का भेद कर्मातीत संन्यासी के लिए नहीं होता जिसने कर्तापन के भाव, फल की इच्छा और अहंभाव का त्याग कर लिया है।
कर्मत्यागी संन्यासी को कर्म के प्रति आसक्ति अथवा इच्छा नहीं होती। इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। निष्काम भाव से किये गये कर्म किसी भी काल में बन्धनकारी नहीं हैं।
भगवान् को कर्म फल समर्पित करने वाले व्यक्ति को कर्म बन्धन नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं और समस्त प्राणियों के लिए स्वाभाविक हैं किन्तु संन्यासी समस्त कर्मों के फल का त्याग कर के जीवन यापन करता है।
फलम् - फल। विविध बाह्य तथ्यों की चेष्टायें इसका कारण हैं। अविद्या (अज्ञान) ही इसका कारण है। यह मोहमाया के इन्द्रजाल में फंसाने वाला और भ्रान्त करने वाला है। फल शब्द नष्ट होने वाली किसी वस्तु का संकेत करता है किसी चिरस्थायी अथवा स्थूल पदार्थ को परिलक्षित नहीं करता ।
कर्म-कर्म । शुभ और अशुभ ।
अनिष्टम् -अशुभ, अप्रिय जैसे नरक, पशु जगत् आदि।
इष्टम् - प्रिय अथवा शुभ।
शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे दोनों मिश्र । जिसके मिश्रम् - कारण मनुष्य जन्म है।
विवेक शून्य, ज्ञान ज्योति से अप्रकाशित अज्ञानी व्यक्ति ही इन तीन प्रकार के फलों का भोग करते हैं जिन्होंने पूर्वतः कर्म फल का त्याग नहीं किया था। परम हंस परिव्राजक वास्तविक संन्यासी जो संन्यास की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं, नित्य आत्म तत्त्व में ध्यानस्थ हैं, केवल आत्म-ज्ञान को ही समर्पित हैं और अपने सत्-चित्-आनन्द स्वरूप में वास करते हैं वे इन फलों का भोग नहीं करते क्योंकि ज्ञानाग्नि ने उनकी अविद्या को भस्म कर दिया है और इस के कार्य रूप संसार के बीज को भी जला दिया है।
आत्म-ज्ञान-प्राप्त मुक्त जीव अथवा जीवन्मुक्त ही सर्व कर्म फल त्यागी हो सकता है क्योंकि वह देहातीत है। वह जानता है कि आत्मा सब कर्मों से परे है, अतीत है और केवल अविद्या के कारण कर्म को आत्मा पर आरोपित किया जाता है। देहाभिमानी व्यक्ति कर्म फल का त्याग नहीं कर सकता। वह सोचता है वह कर्ता है, कर्मों को कार्य रूप देने वाला है और कर्मों के फल की इच्छा रखता है अतः इस अभिलाषा की पूर्ति हेतु अर्थात् कर्म फल भोगने हेतु उसे पुनः पुनः इस भवसागर में अवतरित होना पड़ता है।
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ।।१३ ।।
शब्दार्थ : पञ्च-पाँच, एतानि-ये, महाबाहो - हे महाबाहो, कारणानि-कारण, निबोध-जानो, मे—मुझसे, सांख्ये-सांख्य में, कृतान्ते - जहाँ कर्मों का अन्त है, प्रोक्तानि-कहे गये, सिद्धये-सिद्धि के लिए, सर्वकर्मणाम् सब कर्मों की।
अनुवाद : हे महाबाहो, अर्जुन ! समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन में पाँच कारण बताये गये हैं जो कर्मों का अन्त करने वाले हैं। उनको तुम मुझ से जान लो ।
व्याख्या : आत्मा कर्म से सर्वथा मुक्त है। प्रकृति ही सब चेष्टा करती है। आत्मा मौन साक्षी है। वह तटस्थ (समदर्शी) रहता है। संपूर्ण मानवीय चेष्टाओं का मंदिर (भवन) पाँच कारणों का परिणाम है जिनका निरूपण अगले श्लोक में किया जायेगा।
एतानि-ये-जिनका वर्णन किया जाना है। सांख्य-वेदान्त । उपनिषदों में निरूपित आत्म-ज्ञान जो समस्त कमाँ को समाप्त करता है (सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते)।
इसी कारण से 'कृतान्ते' शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। आत्म-ज्ञान उदित होने पर सर्वकर्म परिसमाप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान् ने अध्याय II, श्लोक 46 में कहा है- "आत्म निष्ठ ब्राह्मण के लिए वेदों का उतना ही महत्त्व है जितना बाढ़ ग्रस्त स्थान में रह रहे व्यक्ति का एक जलाशय से है।" पुनः IV. 33. में कहा है- "हे अर्जुन, समस्त कर्मों का अन्त ज्ञान में होता है।" अतः आत्म-ज्ञान प्रदान करने वाला वेदान्त कर्मों का अन्त है। वेदान्त के आदेशों का पालन कर के आत्म ज्ञानी जीवन्मुक्त कृतकृत्य हो जाता है (जिसने सब कर्म कर लिए हैं और अन्य कुछ करने को शेष नहीं रहता) ।
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ।।१४।।
शब्दार्थ : अधिष्ठानम् स्थान, शरीर, तथा और, कर्ता-कर्ता, करणम् - (उपकरण) इन्द्रियाँ, च-और, पृथग्विधम् - विभिन्न प्रकार के, विविधाः - अनेक प्रकार के, च-और, पृथक् पृथक्, चेष्टाः-कर्म, दैवम् अधिष्ठातृ देव, च-और, एव-ही, अत्र-यहाँ, पञ्चमम् -पाँचवाँ ।
अनुवाद : स्थान (शरीर), कर्ता, करण (इन्द्रियाँ), विविध प्रकार के कर्म और पाँचवाँ अधिष्ठातृ देव,
व्याख्या : अब इन पाँचों की विशेषताओं का ज्ञान करो जिनमें शरीर प्रथम है। इसे स्थान अथवा आश्रय कहते हैं। शरीर इच्छा-द्वेष, सुख-दुःख और ज्ञान आदि का आश्रय स्थल है। जीवात्मा विषयों के सम्पर्क में आकर शरीर के माध्यम से सुख-दुःख के अनुभव लेता है। 'अहं' कर्ता अथवा भोक्ता है। प्रकृति चेष्टा करती है किन्तु भ्रम वश मनुष्य अपने ऊपर कर्तृत्व भाव से आरोपित करता है इसीलिए वह कर्ता कहलाता है।
कर्ता-सम्पर्क में आने वाले सीमित प्रतिबन्धकों के गुण, भवं, सम्पदा अथवा प्रकृति को भोगने वाला।
करणं पृथग्विधम् - विविध प्रकार के शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाले श्रोत्रादि कारण, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ और मन ।
दैवम् अधिष्ठातृ देव जैसे नेत्र का अधिष्ठातृ देव सूर्य है तथा अन इन्द्रियों के भी पृथक् पृथक् देवता हैं जिनकी सहायता से इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य करती हैं; भाग्य।
चेष्टा-कर्म करते समय इन्द्रियों अथवा अवयवों में शक्ति की क्रीड़ा। इनमें से किसी एक करण के अभाव में कर्म असम्भव है।
शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ।।१५।।
शब्दार्थ : शरीरवाङ्मनोभिः-शरीर, वाणी और मन से, यत्-जो, कर्म-कर्म, प्रारभते-करता है, नरः- मनुष्य, न्याय्यम् न्यायपूर्ण, वा-अथवा, विपरीतम् न्याय विरुद्ध, वा-अथवा, पञ्च-पाँच, एते-ये, तस्य-उसके, हेतवः-कारण ।
अनुवाद : शरीर, मन और वचन से मनुष्य इस शरीर के द्वारा जो भी न्यायपूर्ण अथवा न्यायविरुद्ध कर्म करता है-ये उसके पाँच कारण हैं।
व्याख्या : न्याय्यम् यथार्थ, धर्म विरुद्ध जो न हो, शास्त्रसम्मत, न्याययुक्त ।
विपरीतम् - विरुद्ध । जो धर्म विरुद्ध हो, शास्त्र विरुद्ध और न्याय विरुद्ध हो (अन्यायपूर्ण हो) ।
यत्कर्म-पलक झपकना और मूँदना आदि जो जीवन के अनिवार्य कर्म हैं, वे न्याययुक्त और विपरीत शब्दों से इङ्गित किये गये हैं क्योंकि वे पूर्व जन्म कृत पाप-पुण्य के फल स्वरूप हैं।
तस्य हेतवः - इसके कारण। प्रत्येक कर्म के कारण। आलोचक तर्क करता है-"पूर्व श्लोक में कहा है कि शरीर, कर्ता, विभिन्न करण आदि प्रत्येक कर्म के हेतुक हैं तो कर्मों में यह भेद कहाँ से आ गया कि 'जो भी कर्म मनुष्य शरीर, वाणी और मन से करता है ?"
यह दोष नहीं है क्योंकि किसी भी कर्म को करने में अन्यों की अपेक्षा शरीर, वाणी और मन-इन तीनों में से एक अधिक प्रधान होता है। देखना, सुनना आदि अन्य चेष्टायें जो जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, वे इनकी अपेक्षा गौण हैं।
इसलिए समस्त कर्म तीन प्रकार से विभक्त हैं और शरीर, वाणी और मन द्वारा किये जाने वाले हैं। कर्म का फल भी शरीर, वाणी और मन से भोगा जाता है और इनमें एक, अन्य दो की अपेक्षा अधिक प्रधान होता है। इसलिए यह कथन उचित ही है-"शरीर वामनोभिर्यत्कर्म...।"
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ।।१६ ।।
शब्दार्थ : तत्र-वहाँ, एवम् - इस प्रकार, सति-होते हुए, कर्तारम् - कर्ता को, आत्मानम्-आत्मा को, केवलम् -केवल, तु-निश्चित रूप से, यः जो, पश्यति-देखता है, अकृतबुद्धित्वात्-अपरिष्कृत् बुद्धि के कारण, न - नहीं , सः वह, पश्यति-देखता है, दुर्मतिः- विपरीत बुद्धि वाला।
अनुवाद : अब, इस प्रकरण में जो असंस्कृत (अपरिष्कृत) बुद्धि से युक्त अज्ञानी मनुष्य आत्मा को, जो कि पृथक् है, कर्ता मानता है ऐसा विपरीत बुद्धि वाला मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता ।
व्याख्या : आत्मा सदा निष्क्रिय रहता है। आकाश की भाँति वह अनासक्त है। नित्य मौन साक्षी है। कर्मों का द्रष्टा है। देहाभिमानी मनुष्य ही स्वयं को कर्ता मान कर कर्म के बन्धन में पड़ता है और कर्म फल भोगने के लिए पुनः पुनः जन्म लेता है। शरीर को ही चेतन स्वरूप, ईश्वर अथवा आत्मा मानने वाला तो निस्सन्देह उसी आत्मा को ही कर्ता मानेगा। देह में आत्मा का अध्यास करने वाला, देह को ही शुद्ध आत्मा मानने वाला तो नितान्त अन्धकार पूर्ण अज्ञान का जीवन जीता है क्योंकि उसने अपने ऊपर अविद्या का आवरण डाल रखा है। वह कर्मों की श्रृंखला से बंध जाता है और सदा अपने शरीर रूपी पिंजरे में बन्द रहता है।
जिस मनुष्य की बुद्धि के साथ तादात्म्यता नहीं है, जिसकी बुद्धि असंस्कृत अथवा कुत्सित है, जो आत्मा को कर्म करने वाला कर्ता मानता है, वह निश्चित रूप से विपरीत बुद्धि वाला है। वह भ्रमित है; वस्तुतः वह अन्धा है। आँखें होते हुए भी वह नहीं देखता । वह वस्तु का सार रूप नहीं देखता। उसे उस परम तत्त्व का कोई ज्ञान नहीं है जो स्वयं कर्म रहित है, जो सब मनुष्यों के समस्त प्राणियों के अवयवों और अन्तःकरण की चेष्टाओं का साक्षी द्रष्टा है, जो अन्तःकरण, अवयव, प्राण शक्ति और शरीरों को उसी प्रकार कर्म में प्रेरित करता है जैसे चुम्बक एक लौह खण्ड को गति करने के लिए प्रेरित करता है। वह मनुष्य कर्म और आत्मा के सत्य को नहीं जानता।
दुर्मतिः-कुत्सित बुद्धि। विपरीत बुद्धि अथवा अविकसित बुद्धि वाला मनुष्य। वह स्वयं को ही कर्ता मानता है। वह सत्य को समझने में असमर्थ होता है। आत्म-प्रकाश, शुद्ध, कर्म रहित निष्क्रिय आत्म तत्त्व का उसे किंचिदपि ज्ञान नहीं है।
अविद्या में पड़ा दुर्बुद्धि मनुष्य पाँच कारणों के साथ तादात्म्य स्थापित कर के निष्क्रिय आत्मा को कर्मों का कर्ता समझता है जब कि कर्मों के करने वाले वास्तविक करण, पाँच कारण ही हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? वह ऐसा क्यों समझता है? क्यों कि उसके पास शुद्ध, परिष्कृत, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। वेदान्त के अभ्यास से उसकी बुद्धि परिष्कृत नहीं हुई है। वह पुरुषार्थ चतुष्टय (III.3) से अनभिज्ञ है। आध्यात्मिक गुरु अथवा आचार्य के न्यायपूर्ण तर्क से उसकी बुद्धि प्रशिक्षित नहीं हुई है।
शुद्ध कर्म रहित आत्मा को कर्ता मानने वाला निश्चित रूप से असंस्कृत बुद्धि वाला है। उसे निष्काम कर्म और आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए वह मूढ़ बुद्धि कहलाता है। उसकी बुद्धि की गति सही दिशा की ओर कर्म नहीं करती। वह विषयों के घने वन में भटकने वाली है। दुष्ट अश्व की भाँति दौड़ने वाली, आवागमन में डालने वाली है। गीता में दिया गया बुद्धि योग पर उपदेश इसे रोकने में अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से सहायक है।
नेत्र होते हुए भी वह वस्तुओं का यथार्थ दर्शन नहीं कर सकता। वह देखता है किन्तु विषयों के बाह्य, स्थूल, भ्रान्त (मायावी), विकारी, नश्वर रूप को ही देखता है। सब के अवलंबन स्वरूप अमृत, अविकारी, आनन्दमय सार रूप के दर्शन वह नहीं करता। वह मनुष्य पीलिया (jaundice) के रोगी की भाँति है जिसे सब कुछ पीला ही दिखता है अथवा तिमिर रोग वाले मनुष्य की
तरह है जिसे अनेक चन्द्र दिखते हैं अथवा ऐसे मनुष्य जैसा है जो दौड़ते हुए बादलों में चन्द्र को भी गति करता हुआ समझता है अथवा ट्रेन में बैठे उस व्यक्ति की भाँति है जो बाहर वृक्षों को देख कर कल्पना करता है कि वृक्ष चल रहे हैं जबकि वास्तव में जिस गाड़ी में वह बैठा है वही गतिशील है। (निरूपण-V.15; XIII.30)
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।।१७ ।।
शब्दार्थ : यस्य-जिसका, न-नहीं, अहंकृतः- अहंभाव, भावः- भाव, बुद्धिः बुद्धि, यस्य-जिसकी, न-नहीं, लिप्यते-लिप्त है, हत्वा मार कर, अपि-भी, सः वह, इमान्-इन, लोकान्-लोकों का, न-नहीं, हन्ति-मारता है, न नहीं, निबध्यते-बन्धन में आता है।
अनुवाद : 'मैं कर्ता हूँ', इस अहंभाव से जो मनुष्य मुक्त है, जिसका अन्तःकरण शुभ-अशुभ के विकार से दोषयुक्त नहीं है वह मनुष्य इन लोकों को (लोगों को) मार कर भी (मारने के पाप से) बन्धन में नहीं आता।
व्याख्या : हे अर्जुन, कर्मातीत और कर्म बन्धन से भी अतीत मनुष्य की विशेषतायें मैं तुम्हें बताता हूँ।
स्वार्थ भाव और अहंभाव जब नष्ट हो जाते हैं, जब इच्छा और व्यक्तिगत लाभ का त्याग हो जाता है तब कर्म मनुष्य को बांध नहीं सकते। वह जानता है कि शरीर के विनाश से आत्मा का विनाश नहीं होता। वह कर्तृत्वभाव 1 से अतीत रहता है। समाज में शान्ति और सन्तुलन बनाये रखने के लिए हिंसा का कार्य भी उसके लिए अनिवार्य सा हो जाता है। बिना किसी कामना के हिंसा भी उस हिंसक व्यक्ति के हनन समान हो जाती है, जिसे समाज की ओर से, संसार में शांति और सन्तुलन के संरक्षण हेतु जज (न्यायाधिकारी) ने प्राणदंड दिया हो ।
जिसकी बुद्धि प्रशिक्षित हो, अन्तःकरण शुद्ध हो और तर्क शक्ति विकसित हो चुकी हो, जिसे शास्त्रों का समुचित ज्ञान हो, जो शास्त्र-ज्ञान को समर्पित हो और न्याय दर्शन के ज्ञान से युक्त हो, जो आचार्यों द्वारा भली भाँति प्रशिक्षित हो वह इस कर्तापन के अहंकार पूर्ण भाव से सर्वथा मुक्त है। वह अच्छी प्रकार से जानता है कि प्रकृति, गुण अथवा निज स्वभाव ही सब कुछ कर रहे हैं। वह सोचता है- “मैं समस्त क्रियाओं का मौन द्रष्टा हूँ। मैं कर्ता नहीं हूँ। ये पाँच (शरीर, कर्ता, करण आदि) जो शुद्ध अक्रिय आत्मा पर अज्ञान वरा अध्यासित हैं, यही कर्मों के कारण हैं। मैं कुछ नहीं करता। इन्द्रियाँ विषयों में विचरण करती हैं। गुण इन्द्रियों के प्रतिरूप में, जो इन गुणों की ही उपज हैं, विचरण करते हैं। मैं गुणों के विभागों का सार और उनकी प्रक्रियाओं को जानता हूँ। मैं वस्तुतः निरवयव हूँ। कर्म मुझ पर आरोपित कैसे हो सकते हैं? मेरे हाथ नहीं, पैर नहीं, टांग नहीं, श्वास नहीं, मन नहीं, मैं सर्वदा शुद्ध बुद्ध हूँ। निरञ्जन हूँ, अचल हूँ और अविकारी हूँ।" वह इस प्रकार कभी पश्चात्ताप नहीं करेगा- "मैंने कोई अनुचित कार्य किया है। मुझे ऐसा करना चाहिए था। मैंन बुरा कर्म कर लिया है। अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा।" वह नित्य बुद्धिमान् है। वह अनुचित कर्म कर ही नहीं सकता। उसकी इच्छा प्रभु की इच्छा हो गई है, वैश्विक इच्छा हो गई है। भगवान् की इच्छा में उसकी इच्छा मिल गई है। वह जो कुछ भी करता है, भगवान् ही करता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। वह यथार्थ देखता है। हनन कर के भी वह हिंसा के कर्म से मुक्त है। उस कर्म के परिणाम के बन्धन में वह नहीं आता। वह शुभ और अशुभ से परे है, द्वन्द्वों से अतीत है क्योंकि वह आत्म ज्ञानी है।
आलोचक कहता है-"मार कर भी नहीं मारता", यह कथन विपरीत है। किन्तु हम कहते हैं-
यह कथन विपरीत नहीं है। लौकिक दृष्टि से मनुष्य, शरीर में आत्म बुद्धि कर के 'मैं मारता हूँ' ऐसा सोचता है किन्तु पारमार्थिक दृष्टि से जैसा कि ऊपर समझाया गया है, भगवान् कहते हैं, वह नहीं मारता और न ही बन्धन में आता है।
एक अन्य आलोचक कहता है-आत्मा शरीर आदि के साथ मिल कर कर्म करता है। 'जो मनुष्य आत्मा को शरीर से पृथक् मान कर भी उसे कर्ता समझता है वह भी अकृत बुद्धि है।' (निरूपण-XVIII.16)
उत्तर है- "यह दोष भी अनुचित है। जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश सूक्ष्मता के न्याय से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार विद्यमान (व्याप्त) होते हुए भी अप्रभावित रहता है। ये अनश्वर अविकारी, अपरिवर्तनशील, निराकार, निर्गुण आत्मा शरीरस्थ होते हुए भी न तो कर्म करता है और न ही कर्म से प्रभावित होता है। जिस प्रकार स्फटिक रक्त वर्ण पुष्प के सम्पर्क में आने पर अप्रभावित रहता है और सूर्य नेत्र रोग से अप्रभावित रहता है उसी प्रकार आत्मा भी इन सब प्रभावों से अतीत है। विकारशील वस्तु ही दूसरे के साथ मिल कर कर्ता बन सकती है। आत्मा सदा पृथक् है, स्वतन्त्र है, मुक्त है। यह आत्मा निर्विकार है (II.25)। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, (III.28)। शरीर में वास करते हुए भी वह कर्म नहीं करता ( III.31)| कर्म गुणों के द्वारा किये जाते हैं (III.27)।" बृहदारण्यकोपनिषद् ( 4.3.7 .) में आता है-
"मानो यह ध्यान करता है। मानो यही गति करता है।" तर्क द्वारा भी हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं।
"यह निरवयव है, भाग रहित है, स्वतन्त्र है, मुक्त है, निर्विकार है। इसलिए शरीर के कर्म आत्मा के कर्तृत्व पर आरोपित नहीं किये जा सकते।"
वस्तुतः एक के कर्म दूसरे के पास नहीं जा सकते जिसने वे कर्म किये ही न हों। जैसे आकाश में आरोपित नीलिमा आकाश की नहीं है, सीप में आरोपित चाँदी सीप की नहीं हो सकती, मृग मरीचिका में जल नहीं हो सकता इसी प्रकार अविद्या के कारण आत्मा पर आरोपित विकार आत्मा के नहीं हो सकते। शरीर में होने वाले विकार शरीर के ही हैं, शुद्ध आत्म तत्त्व के नहीं हैं जो सदा साक्षी रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए यह कथन सही है कि विवेकी मनुष्य जो अन्तःकरण की अशुद्धियों और अहंभाव से मुक्त है न तो हिंसा करता है और न ही हिंसा करने पर बन्धन में आता है।"
अध्याय II.19. में भगवान् ने कहा था- "वह न तो मारता है और न ही मारा जाता है", 11.20. में उन्होंने कहा- "आत्मा अजन्मा, शाश्वत, नित्य, सनातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरता।" इतस्ततः भगवान् ने स्पष्ट किया है कि आत्मा कर्म से प्रभावित नहीं होता और बुद्धिमान् मनुष्य को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वे अन्त में कहते हैं- "ज्ञानी न तो मारता है, न बन्धन में आता है", और इसी से गीता का उपदेश समाप्त होता है। अहंभाव से मुक्त संन्यासी कर्म से प्रभावित नहीं होते। कर्मों के त्रिविध परिणाम-शुभ, अशुभ और मिश्र (श्लोक १२), उनके लिए नहीं हैं। कर्म से तो सांसारिक मनुष्य ही लिप्त होते हैं क्योंकि वे अहंभाव से और फल की आशा से युक्त होते हैं। वे कर्म फल भोगने के लिए बाध्य होते हैं इसलिए उन्हें पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। (निरूपण –II.19; V.7)
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ।।१८ ।।
शब्दार्थ : ज्ञानम् ज्ञान, ज्ञेयम्-जानने योग्य, परिज्ञाता-ज्ञाता (जानने वाला), त्रिविधा-तीन प्रकार के, कर्मचोदना-कर्मों की प्रेरणा, करणम् -इन्द्रियाँ, कर्म-कर्म, कर्ता-कर्ता, इति-इस प्रकार, त्रिविधः-तीन प्रकार के, कर्मसंग्रहः कर्म के संग्रह (संचय) ।
अनुवाद : ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, यह तीन कर्म के प्रेरक हैं। करण (इन्द्रियाँ), कर्म और कर्ता, यह तीन कर्म के संघटक अर्थात् कर्म संग्रह हैं।
व्याख्या : ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता करने योग्य पदार्थ अर्थात् ज्ञेय, सम्मिलित रूप से संसार के बीज रूप हैं। इसे त्रिपुटी कहते हैं। इन तीनों का संयोग मनुष्य को शारीरिक, वाचिक और मानसिक, यह त्रिविध कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यह त्रिपुटी मनुष्य की क्रियाओं की संचालन शक्ति है। वह मनुष्य मधुर स्वादिष्ट मिष्टान्न देख कर तो हर्षित होता है किन्तु कोबरा अथवा सिंह को देख कर भयभीत हो जाता है। रुचिकर अथवा अरुचिकर विषयों को देख कर वह प्रभावित होता है और अनुकूल को ग्रहण करने का और प्रतिकूल को दूर करने का प्रयास करता है।
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार-ये चार मिल कर अन्तःकरण कहलाता है। कर्ण, त्वचा, जिह्ना, नासिका और नेत्र-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इन पाँच इन्द्रियों से प्रेरित हो कर जीवात्मा कर्म में प्रवर्तित होता है। वह पाँच कर्मेन्द्रियों-वाणी, हस्त, पाद, गुदा और उपस्थ की सहायता से कार्य करता है।
ज्ञानम् -कोई भी ज्ञान । सामान्य भाव में सर्व पदार्थ विषयक ज्ञान ।
ज्ञेयम्-जानने में आने वाला पदार्थ । समस्त सामान्य पदार्थ ।
परिज्ञाता-ज्ञाता, अनुभव कर्ता, भोक्ता। अविद्यायुक्त मनुष्य जो सीमित प्रतिबन्धकों की प्रकृति को धारण किये हुए है।
"यह त्रिपुटी समस्त कर्मों के प्रति त्रिविध प्रेरणा करती है। किसी भी कर्म की प्रवृत्ति, प्राप्त करने अथवा त्यागने की, तभी सम्भव है जब ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की त्रिपुटी हो।
करणम् - इन्द्रियाँ (साधन)। जिनके द्वारा कर्म किया जाता है।
कर्म के पाँच कारणों-शरीर आदि द्वारा किये गये कर्म, जो अपने-अपने स्थान के अनुरूप तीन वर्गों-मन, वाणी और शरीर में विभक्त हुए इन्द्रिय आदि के अन्योन्य संसर्ग व चेष्टा से है।
कर्ता-करने वाला। इन्द्रियों (करणों) को अपने-अपने कर्म में नियुक्त करने वाला अर्थात् जीव जो सीमित प्रतिबन्धों की प्रकृति वाला प्रतीत होता है और शरीर रूपी वाहन में रह कर चेष्टा करता है। समस्त कर्म इन तीनों के कारण सम्पादित होते हैं-कर्ता, कर्म और करण (इन्द्रियाँ) । इसलिए ये कर्म के त्रिविध संघटक हैं।
कर्म, कारक और फल, ये त्रिगुणात्मक होने से भगवान् इन का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं।
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ।।१९ ।।
शब्दार्थ : ज्ञानम् - ज्ञान, कर्म-कर्म, च-और, कर्ता-कर्ता, च-और, त्रिधा-तीन प्रकार का, एव-ही, गुणभेदतः- गुणों के भेद से, प्रोच्यते-कहे जाते हैं, गुणसंख्याने गुणों के विज्ञान में (सांख्य दर्शन) को, यथावत्-जैसे हैं, वैसे ही, शृणु-सुनो, तानि उनको, अपि भी।
अनुवाद : ज्ञान, कर्म और कर्ता सांख्य दर्शन में गुणों के भेद से कहे गये हैं। उनको भी यथावत् सुनो अर्थात् जैसा शास्त्रविहित है वैसा ही सुनो।
व्याख्या : अपनी विशेष प्रकृति के साथ तीनों गुण सम्पूर्ण विश्व को अपने आधीन किये हुए हैं। गुण की प्रधानता के अनुसार कर्ता, कर्म और ज्ञान की प्रकृति त्रिविध है। यदि तीनों सात्त्विक हैं तो कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होंगे।
कर्ता-कर्म को करने वाला।
गुणों के विज्ञान से यहाँ अभिप्राय कपिल मुनि के न्याय शास्त्र से यद्यपि सर्वोच्च सत्य के विषय में सांख्य दर्शन वेदान्त के विपरीत है अनंत अद्वैतवाद का इसमें विरोध है तथापि गुणों के विषय में यह प्रामाणिक है।
मैं ज्ञान, कर्म और कर्ता तथा विभिन्न गुणों के कारण उनके विविध भेलें का वैज्ञानिक रूप से तथा न्यायानुसार विवेचन करूँगा। हे अर्जुन, अत्यन्न ध्यानपूर्वक मेरे उपदेशों को सुनो। तुम्हारा कल्याण होगा।
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ।।२० ।।
शब्दार्थ : सर्वभूतेषु सब प्राणियों में, येन-जिसके द्वारा, एकम् - एक, भावम् -सत्य, अव्ययम् - अनश्वर, ईक्षते-देखता है, अविभक्तम् -सम्पूर्ण, अखण्ड, विभक्तेषु पृथक् पृथक् (प्राणियों में), तत्-उस, ज्ञानम् - ज्ञान को, विद्धि-जानो, सात्त्विकम् सात्त्विक ।
अनुवाद : वह (ज्ञान) जिसके द्वारा मनुष्य विभक्तों में अविभक्त उस एक अनश्वर सत्य-स्वरूप परमात्मा को देखता है उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो ।
व्याख्या : वह ज्ञान शुद्ध है जो दृश्य पदार्थों में विभिन्न नहीं देखता। दृश्य जगत् की दृश्यमान विभिन्नता में द्रष्टा उस सर्वव्यापक, अमृत-तत्त्व के ही दर्शन करता है। वह विविधता में एकता, अनेकता में एकता और सब में एक को देखता है। वह देखता है कि सब पदार्थ उसी एक सार तत्त्व में मूल बद्ध हैं।
भावम् -सत्य । एक आत्मा ।
सर्वभूतेषु सब प्राणियों में। अव्यक्त से लेकर चराचर जगत् पर्यन्त ।
अव्ययम् अनश्वर, अक्षय्य, अविकारी, जो न तो स्वयं में क्षीण हो सकता है न गुणों में। वह निर्विकारी है।
जिस प्रकर आकाश अविभाज्य है उसी प्रकार आत्मा भी अविभाज्य है, उसके भाग नहीं हो सकते। सब शरीरों में आत्मा वही है। सब प्राणियों में यही चेतना है। विविध शरीरों में चेतना विभिन्न नहीं है। यह एक समन्वित, अखण्ड सार तत्त्व है जो सब शरीरों में सब प्राणियों में विद्यमान है। हे अर्जुन, इस अपरोक्ष और यथार्थ दर्शन को अद्वैत तत्त्व का सात्विक (पवित्र) दर्शन ■ जानो। (निरूपण - IV.35; VI.29; XIII. 16, 28; XVIII.30)
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ।।२१ ।।
शब्दार्थ : पृथक्त्वेन अन्योन्य पृथक्ता के कारण, तु-किन्तु, यत्-जो, ज्ञानम् - ज्ञान, नानाभावान् विविध भावों को, पृथग्विधान् - विविध प्रकार के, बेति-जानता है, सर्वेषु सब में, भूतेषु-प्राणियों में, तत्-वह, ज्ञानम् -ज्ञान, विद्धि-जानो, राजसम् राजसिक ।
अनुवाद : किन्तु वह ज्ञान जो समस्त प्राणियों में एक-दूसरे की पृथक्ता के कारण उनमें अस्तित्व की पृथक्ता देखता है वह राजसिक है।
व्याख्या : ज्ञान जो देखता है-ज्ञान में कर्तापन का अभाव होने के कारण उसका अभिप्राय ऐसे लेना चाहिए- ज्ञान, जिसके द्वारा मनुष्य देखता है।
भावान् -आत्मा अथवा अस्तित्व ।
पृथग्विधान् - एक-दूसरे से पृथक् । भिन्न-भिन्न शरीरों में पृथक् अस्तित्व दर्शन करना।
द्वैत दर्शन कराने वाला ज्ञान राजसिक है। नानाविध सृष्टि को पृथकत्व के आवरण से आवृत कर के प्रकृति विद्वान् पुरुष को भी भ्रमित करती है। राजसिक ज्ञान वश प्राणी पृथक् पृथक् दिखते हैं और एकत्व का दर्शन भी लुप्त हो जाता है। वह ज्ञान जो सृजित पदार्थों में विविधता और अनेकता देखता है और उनके आकार और परिमाण के अनुरूप उनमें छोटा-बड़ा देख कर पृथक्ता देखता है वह राजसिक ज्ञान है और कलुषित है। राजसिक ज्ञान से युक्त मनुष्य सर्वत्र विविधता देखता है वह केवल अनेक ही देखता है।
हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें तामसिक ज्ञान के विषय में उपदेश करूँगा जिससे तुम उसका निराकरण कर सको ।
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् ।
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ।।२२ ।।
शब्दार्थ: यत्-जो, तु किन्तु, कृत्स्नवत् -मानो पूर्ण, एकस्मिन् - एक (में), कार्य-कार्य में, सक्तम् - आसक्त, अहैतुकम् - बिना कारण (हेतु) के, अतत्वार्थवत् वास्तविकता के ज्ञान से शून्य, अल्पम्-तुच्छ, च-और, तत्वह, तामसम् - तामसिक, उदाहृतम् -कहा गया है।
अनुवाद : किन्तु जो ज्ञान किसी एक कार्य में सम्पूर्ण की भाँति आसक्त है और जो हेतु रहित, तत्त्व रहित है और तुच्छ है वह ज्ञान तामसिक है।
व्याख्या : जो ज्ञान प्रत्येक वस्तु अथवा प्राणी के अस्तित्व को स्वयं में पूर्ण मानता है वह तामसिक है।
एकस्मिन् कार्य-किसी एक कार्य में जैसे शरीर, इसे आत्मा मान लिया जाये, कोई प्रतिमा-उसे भगवान् माना जाये और यह सोचें कि इससे उच्चतर अन्य कुछ नहीं।
दिगम्बर जैनी मानते हैं कि आत्मा शरीर में रहने वाला है और शरीर के ही आकार का है। कुछ मानते हैं कि पत्थर का टुकड़ा अथवा काष्ठ खण्ड ही ईश्वर है। यह किसी एक कार्य में आसक्त ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान युक्ति-युक्त अथवा न्याय पर आधारित नहीं है। यह ज्ञान तत्त्व दर्शन से शून्य है। यह अल्प ज्ञान है क्योंकि यह न्याय सङ्गत नहीं है। यह तुच्छ परिणाम देने वाला है। यह एक सीमित क्षेत्र तक व्याप्त है, सर्वज्ञता की दृष्टि से अत्यल्प है। यह तामसिक ज्ञान है क्योंकि तामसिक वृत्ति वाले मनुष्यों में ऐसा ज्ञान होता है जो विवेक शून्य होते हैं।
नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।। २३ ।।
शब्दार्थ : नियतम् - नित्य, सङ्गरहितम् - आसक्ति रहित, अरागद्वेषतः - राग-द्वेष रहित, कृतम् - किया गया, अफलप्रेप्सुना-फल की इच्छा न करने वाले के द्वारा, कर्म-कर्म, यत्-जो, तत्-वह, सात्विकम् - सात्त्विक, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : फल की आकाङ्क्षा न रखने वाले पुरुष के द्वारा किया गया नित्य कर्म जो आसक्ति रहित है और राग-द्वेष से रहित है-वह सात्त्विक है।
व्याख्या : नियतम् - नित्य । शास्त्र विहित कर्म। नित्य कर्म राग अथवा द्वेष से प्रेरित हो कर नहीं किया जाता।
यह पावन कर्म है। ऐसे पवित्र कर्म को करने वाला अत्यन्त आह्लाद का अनुभव करता है। वह अपना कर्तव्य अथवा अन्य कोई कोई भी कार्य पूर्ण मन से करता है। फल की इच्छा न रखते हुए वह स्वेच्छा से हरि चरणों में कर्म फल समर्पित करता है। हे अर्जुन, अब मैं राजसिक कर्म की प्रकृति का वर्णन करूँगा। ध्यान पूर्वक तुम श्रवण करो।
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ।।२४ ।।
शब्दार्थ : यत्-जो, तु-किन्तु, कामेप्सुना-फल की इच्छा रखने वाले के द्वारा, कर्म-कर्म, साहंकारेण-अहंकार से युक्त, वा-अथवा, पुनः-फिर, क्रियते-किया जाता है, बहुलायासम्-बहुत परिश्रम से, तत्-वह, राजसम् राजसिक, उदाहृतम् -कहा जाता है।
अनुवाद : किन्तु जो कर्म इच्छा पूर्ति के लिए अथवा मिथ्या अहंकार वश अथवा कठिन परिश्रम से किया जाता है वह राजसिक कर्म कहा जाता है।
व्याख्या : राजसिक मनुष्य विभिन्न स्वार्थ-कर्म करता है। जनगण में वह अपने कार्यों का मिथ्या अहंकार दिखाता है। रजस् ही उसे वैसा करने को प्रेरित करता है। फल की इच्छा त्याग कर तो वह कर्म कर ही नहीं सकता।
कामेप्सुना, फलेप्सुना-राजसिक मनुष्य कर्मों के फल में सुख खोजता है। केवल जीवन्मुक्त ही पूर्णतया अहंकार-शून्य हो सकता है। वह तो स्वप्न में भी फल की इच्छा नहीं कर सकता क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार कर के वह आप्तकाम हो जाता है। उसकी समस्त कामनायें पूर्ण हो जाती हैं। (आप्तकामस्य का स्पृहा ?) आत्म-ज्ञान की अग्नि से जिस ज्ञानी में समस्त कामनायें सन्तुष्ट हो चुकी हैं अथवा भस्म हो चुकी हैं, उसमें कामना कहाँ से आ सकती है?
सात्त्विक कर्म करने वाला भी आत्म-ज्ञान के अभाव में अहंकार से युक्त होता है। यदि ऐसा है तो राजसिक और तामसिक कर्म-कर्ता तो और अधिक अहंकारी होते हैं। लौकिक भाषा में किसी ज्ञानी पण्डित के विषय में हम कहते हैं-"यह पण्डित अत्यन्त विनम्र है, कुछ भी ग्रहण न करने वाला और अनहंकारी ब्राह्मण है।"
हे अर्जुन, अब तामसिक कर्म की विशेषतायें सुनो।
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।।२५ ।।
शब्दार्थ : अनुबन्धम् - भावी परिणाम, क्षयम् -विनाश, हानि, हिंसाम् - हिंसा को, अनपेक्ष्य-विचार न कर के, च-और, पौरुषम् -सामर्थ्य, मोहात् - मोह बश, आरभ्यते-किया जाता है, कर्म-कर्म, यत्-जो, तत्-वह, तामसम् तामसिक, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : जो कर्म मोह वश भावी परिणाम, हानि, हिंसा और अपनी सामर्थ्य का विचार न कर के किया जाता है वह कर्म तामसिक कहा जाता है।
व्याख्या : तामसिक कर्म दूसरों को हानि पहुँचाते हैं। तामसिक मनुष्य यह विचार कदापि नहीं करता कि जो कर्म वह करने लगा है उसे करने की उसमें सामर्थ्य भी है अथवा नहीं, वह तो मानो आँख मूंद कर व्यर्थ के कर्म में संलग्न रहता है। नितान्त विचार शून्यता के कारण वह किसी भी आभास अथवा भावी परिणाम को न देखते हुए अथवा कर्म की आने वाली कठिनाई को न सोचते हुए कर्म प्रारम्भ कर देता है। अपने अहंकारपूर्ण ढंग से वह कार्य करता जाता है। अच्छा-बुरा और 3747 - 4(14) का भी विवेक न कर के वह आगे बढ़ता जाता है।
क्षयम् -किसी कर्म के परिणाम स्वरूप शक्ति और धन की हानि ।
हिंसा-प्राणियों को पीड़ा पहुँचाना ।
पौरुषम् - अपनी योग्यता अथवा कर्म समाप्ति की सामर्थ्य ।
अब सात्त्विक कर्ता के गुणों का श्रवण करो। अब भगवान् कर्ता के भेद पर उपदेश करते हैं।
मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।
सिद्ध्यसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ।। २६ ।।
शब्दार्थ : मुक्तसङ्गः- आसक्ति रहित, अनहंवादी- अहंकार रहित, धृत्युत्साहसमन्वितः - दृढ़ संकल्प और उत्साह से पूर्ण, सिद्ध्यसिद्धयोः-सफलता और असफलता में, निर्विकारः- विकार रहित (अप्रभावित), कर्ता-कर्ता, सात्त्विक सात्त्विक, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : जो कर्ता आसक्ति रहित है, अहंकार शून्य है, दृढ़ संकल्प और उत्साह से युक्त है और सफलता-विफलता में उद्विग्न नहीं होता, सम रहता है, वह सात्त्विक है।
व्याख्या : सात्त्विक कर्ता अभिमान त्याग कर पूर्ण मन से कर्म करता है। वह समुचित देश, काल की प्रतीक्षा करता है और शास्त्रों के निर्देशानुसार विश्वय करता है कि अमुक कार्य करणीय है अथवा नहीं। वह आत्म शक्ति और उत्साह को विकसित करता है। वह भौतिक सुखों की आकाला नहीं करता। किसी भी शुभ कार्य के लिए वह अपना जीवन उत्सर्ग करने को उद्यत रहता है। सफलता में वह हर्षित नहीं होता और विफलता में दुःखी नहीं होता। कोई भी कार्य करते समय उसका मन सन्तुलित रहता है। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष, हे अर्जुन, सात्त्विक कहलाता है।
सिद्धि-सफलता, कृत कर्म का परिणाम।
निर्विकारः-अप्रभावित । शास्त्रों के आधिपत्य से प्रेरित हो कर कर्म करने वाला, फल की इच्छा से नहीं।
हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें राजसिक कर्ता के गुण बताऊँगा।
रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।।२७ ।।
शब्दार्थ : रागी-आसक्त, कर्मफलप्रेप्सुः-कर्म फल की इच्छा रखने वाला, लुब्धः- लोभी, हिंसात्मकः - दूसरों को कष्ट देने वाला, अशुचिः-अपवित्र, हर्षशोकान्वितः- हर्ष और शोक में विचलित होने वाला, कर्ता-कर्ता, राजसः- राजसिक, परिकीर्तितः-कहा जाता है।
अनुवाद : राग युक्त (आसक्त), फल की कामना रखने वाला, लोभी, अत्याचारी, अपवित्र, हर्ष-शोक में विचलित होने वाला-ऐसा कर्ता राजसिक कहलाता है।
व्याख्या : राजसिक कर्ता सम्पूर्ण संसार के पदार्थों का लोभी और पापों का मानो आश्रय है। सांसारिक फल-प्राप्ति हेतु जहाँ कहीं भी उसकी कल्पना उड़ान भरती है वहीं पहुँच कर वह अनन्यमनस्क भाव से उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो कुछ भी वह प्राप्त करता है वह केवल अपने और अपने परिवार तक सीमित रखता है। कर्म फल मिल जाये तो प्रमुदित होता है और यदि उसका प्रयास असफल हो जाये तो शोक करता है।
लुब्धः- लोभी। दूसरे के धन की तृष्णा करने वाला । योग्य पात्र को भी अपना धन न देने वाला।
हिंसात्मकः दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाला।
अशुचिः- अपवित्र । अन्तः बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धि से रहित। (काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से रहित होना और हृदय में दया, करुणा, क्षमा, अनासक्ति और प्रेम गुणों का विकास करना आन्तरिक शुद्धि है।)
हर्ष शोकान्वितः - प्रिय (अनुकूल) की प्राप्ति पर हर्षित होना और अप्रिय (प्रतिकूल) की प्राप्ति पर शोक करना अथवा प्रिय से वियोग में विचलित होना। ऐसा व्यक्ति सफलता में प्रसन्न होगा और विफलता में विलाप करेगा।
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ।।२८ ।।
शब्दार्थ : अयुक्तः अस्थिर, प्राकृतः-संस्कारहीन (असभ्य), स्तब्ध:- हठी, शठः-कपटी, नैष्कृतिकः-ईर्ष्यालु, अलसः आलसी, विषादी- अवसाद युक्त (निराशायुक्त), दीर्घसूत्री-विलम्ब से कार्य करने वाला, च-और, कर्ता- कर्ता, तामसः-तामसिक, उच्यते-कहा जाता है।
अनुवाद : अस्थिर चित्त वाला, संस्कार हीन, हठी, कपटी, ईर्ष्यालु, आलसी, अवसाद युक्त, दीर्घ सूत्री अर्थात् कर्तव्य में विलम्ब करने वाला-ऐसा कर्ता तामसिक कहा जाता है।
व्याख्या : असभ्य प्रकृति का होने के कारण वह विहित और निषिद्ध कर्मों में विवेक बुद्धि नहीं रखता। उसका हृदय मिथ्या अभिमान से पूर्ण होता है। किसी ज्ञानी अथवा देवता के समक्ष वह प्रणाम नहीं करेगा। वह आचार-व्यवहार में अत्यन्त हठी होता है, दण्ड की भाँति सीधा रहेगा, झुकेगा नहीं। वह धोखेबाज और जुआ (द्यूत क्रीड़ा) आदि बुरे गुणों से युक्त होता है। बुरे कर्म करने को वह सदा उद्यत रहता है। कुछ शुभ कर्म करने का अवसर हो तो वह पूर्णतया निष्क्रिय और आलसी हो जाता है। किन्तु बुरा करने में वह सदैव जागरूक है।
प्राकृतः - असभ्य । संस्कार विहीन बुद्धि से युक्त और बालक की भाँति व्यवहार करने वाला।
स्तब्धः - दण्ड की भाँति न झुकने वाला। किसी को भी प्रणाम न करने वाला।
शठः दुष्ट । अपनी वास्तविक प्रकृति को छिपाने वाला।
नैष्कृतिकः- लोगों में छोटी-छोटी बात पर झगड़ा करवाने वाला । अलसः आलसी । कर्तव्य कर्म को भी न करने वाला।
दीर्घसूत्री-अपने कार्य को कल तक छोड़ने वाला। सदा आलस्य से और युक्त, कर्तव्य कर्म को मास भर में भी समाप्त न करने वाला।
बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ।।२९ ।।
शब्दार्थ : बुद्धेः बुद्धि का, भेदम्-भेद, घृतेः दृढ़ता का, च-और, एव-ही, गुणतः गुणों के अनुसार, त्रिविधम्-तीन प्रकार का, शृणु-सुनो, प्रोच्यमानम् जो कहा जा रहा है, अशेषेण-पूर्ण रूप से, पृथक्त्वेन पृथक् रूप से, धनञ्जय- हे धनञ्जय ।
अनुवाद : हे अर्जुन, अब तुम गुणों के अनुरूप बुद्धि और धृति के त्रिविध स्वरूप को पूर्णता से और पृथक् पृथक् रूप से, मुझसे सुनो।
व्याख्या : धनञ्जय-धन को जीतने वाला। अर्जुन का नाम । दिग्विजय काल में धरती की चारों दिशाओं से अर्जुन ने प्रचुर आध्यात्मिक और भौतिक सम्पदा अर्जित की थी इसलिए उसका नाम धनञ्जय पड़ा।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ।।३० ।।
शब्दार्थ : प्रवृत्तिम् -कर्म, बन्धन के हेतु कर्म मार्ग, च-और, निवृत्तिम् -मोक्ष का हेतु संन्यास मार्ग, च-और, कार्याकार्ये-कर्तव्य (करने योग्य) और अकर्तव्य (न करने योग्य) कर्म में, भयाभये-भय और अभय में, बन्धम् बन्धन को, मोक्षम् मोक्ष, च-और, या-जो, वेत्ति - जानती है, बुद्धिः - बुद्धि, सा-वह, पार्थ- हे पार्थ, सात्त्विकी -सात्त्विक है।
अनुवाद : जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति के पथ को, कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों को, भय और अभय तथा बन्धन और मोक्ष को जानती है, हे अर्जुन वह सात्त्विक बुद्धि है।
व्याख्या : ज्ञान की त्रिविध प्रकृति श्लोक २२ में बताई जा चुकी है। अब बुद्धि की त्रिविध प्रकृति का वर्णन किया जाता है। ज्ञान, बुद्धि से पृथक् है।
प्रवृत्ति-कर्म । बन्धन का कारण । कर्म का मार्ग।
निवृत्ति-अकर्म । मोक्ष का कारण । संन्यास मार्ग ।
कार्याकार्य-देश-काल विशेष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान सात्त्विक बुद्धि में होता है। दृष्ट अथवा अदृष्ट परिणाम देने वाले कर्मों का भी इसे ज्ञान होता है। शास्त्र सम्मत और शास्त्र-निषिद्ध कर्मों का ज्ञान भी सात्त्विक बुद्धि में रहता है। शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट जीवन के नित्य के क्रिया कलापों को करने वाले व्यक्ति का यह सात्विक बुद्धि मार्गदर्शन करती है।
भयाभये-भय और निर्भयता । भय का और अभय का दृष्ट अथवा अदृष्ट कारण।
बन्धमोक्षम् - बन्धन और मोक्ष कारणों सहित ।
ज्ञान बुद्धि की एक वृत्ति (अवस्था विशेष) है जब कि बुद्धि कर्म में संलग्न होती है अथवा अवस्था के विकार को प्राप्त होती है। धृति भी बुद्धि की एक विशेष वृत्ति (अवस्था) है। (निरूपण - XVIII.20)
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।।३१ ।।
शब्दार्थ : यया-जिसके द्वारा, धर्मम् - धर्म, अधर्मम् - अधर्म, च-और, कार्यम् -कर्तव्य कर्म, च-और, अकार्यम् - अकर्तव्य कर्म, एव-ही, च-और, अयधावत् - अयथार्थ रूप से, प्रजानाति-जानती है, बुद्धिः बुद्धि, सा-वह, पार्थ-हे पार्थ, राजसी -राजसिक है।
अनुवाद : हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म और अधर्म को तथा करने योग्य कर्म और न करने योग्य कर्म को यथार्थ रूप से नहीं जानती अर्थात् इनके भेद को नहीं जानती वह बुद्धि राजसिक है।
व्याख्या : धर्म शब्द के समकक्ष आंग्ल भाषा में कोई शब्द नहीं मिलता। कर्तव्य, सदाचार, गुण, न्याय आदि धर्म शब्द के अभिप्राय को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करते। वह जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर अर्थात् ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्म-ज्ञान के लिए प्रेरित करे वह धर्म है। अविद्या के गभीरगर्त (गड्ढे) में नीचे गिराने वाला अथवा अध: पतन कराने वाला अधर्म है। शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेश धर्म हैं। शास्त्रों में प्रतिषिद्ध संदेश अधर्म है। राजसिक बुद्धि धर्म और अधर्म अथवा यथार्थ-अयथार्थ कर्म का भेद करने में असमर्थ होती है।
अयथावत् अनुचित ढंग से । सर्वोच्च ज्ञान के द्वारा, विद्वान् के द्वारा अथवा सर्वतो भाव से निर्णीत भाव के विपरीत भाव को अयथावत् कहते हैं।
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता ।
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।। ३२ ।।
शब्दार्थ : अधर्मम्-अधर्म, धर्मम्-धर्म, इति-इस प्रकार, या-जो, मन्यते मानता है, तमसा-अन्धकार से, आवृता-आच्छादित, सर्वार्थान्-समस्त वस्तुओं को, विपरीतान् विपरीत, च-और, बुद्धिः बुद्धि, सा-वह, पार्थ-हे पार्थ, तामसीतामसिक (तमोगुण से युक्त) ।
अनुवाद : हे अर्जुन ! तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और अन्य सब पदार्थों को भी विपरीत ही देखती है वह तामसिक है।
व्याख्या : वह बुद्धि जो धार्मिक कृत्य को बुराई समझती है, यथार्थ को मिथ्या और प्रत्येक यत्न विपरीत दिशा में करती है, गुण को अवगुण और शास्त्र विहित सत्य को अनुचित कहती है वह तामसिक है। यह प्रत्येक वस्तु को विपरीत भाव में ग्रहण करती है।
इस प्रकार, हे अर्जुन, मैंने बुद्धि के तीन प्रकार तुम्हें बताये हैं। अब धृति की त्रिविध चर्चा करते हैं।
धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः ।
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ।।३३ ।।
शब्दार्थ : धृत्या-धृति (संकल्प) द्वारा, यया-जिस (के द्वारा), धारयते-धारण करता है, मनः-मन, प्राणेन्द्रियक्रियाः - प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को, योगेन-योग के द्वारा, अव्यभिचारिण्या-अविचल, धृतिः- धृति, सा-वह, पार्थ-हे पार्थ (अर्जुन), सात्त्विकी-सात्त्विक है।
अनुवाद : जिस अव्यभिचारिणी अर्थात् अचल, स्थिर धृति के द्वारा समाधि योग से मन प्राण और इन्द्रियों की समस्त चेष्टायें संयत की जाती हैं वह धृति, हे पार्थ, सात्त्विक है।
व्याख्या : मन में जब धारणा जाग्रत की जाती है तो मन, प्राण और इन्द्रियों के क्रिया कलाप नियन्त्रित हो जाते हैं। इन्द्रियाँ मन में संहत हो जाती हैं। प्राण और अपान सुषुम्णा नाड़ी में चलने लगते हैं।
योग-समाधि अथवा मन की एकाग्रता । केवल धारणा के द्वारा तुम मन प्राण और इन्द्रियों को वशीभूत नहीं कर सकते। मन की एकाग्रता के साथ संयुक्त धृति (संकल्प) के द्वारा ही तुम इन्हें नियन्त्रित कर सकते हो।
अविचल धृति के द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियों का निग्रह हो जाये तो वे बाह्य विषयों की ओर उन्मुख नहीं हो सकते, कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकते, शास्त्र विरुद्ध पथ का अनुसरण नहीं कर सकते, वे अपने-अपने मूल कारणों में विलीन हो जायेंगे, उनकी बहिर्मुखी वृत्तियाँ सर्वथा निग्रहीत हो जायेंगी। यह धृति कोई दबाव अथवा प्रतिरोध नहीं है प्रत्युत् एक विवेकपूर्ण विलय अथवा आन्तरिक रूपान्तरण है।
यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।
प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ।।३४ ।।
शब्दार्थ : यया-जिसके द्वारा, तु-किन्तु, धर्मकामार्थान् - धर्म, काम और अर्थों को, धृत्या-धृति के द्वारा, धारयते - धारण करता है, अर्जुन-हे अर्जुन, प्रसङ्गेन-आसक्ति के कारण, फलाकाङ्क्षी-फल का इच्छुक, धृतिः- धृति, सा-वह, पार्थ-हे पार्थ, राजसी -राजसिक ।
अनुवाद : किन्तु, हे अर्जुन, आसक्तिवश और फल की इच्छा से युक्त हो कर जब व्यक्ति धर्म, काम और धन-अर्जित करने में संलग्न होता है-उसकी वह धृति राजसिक कही जाती है।
व्याख्या : राजसिक धृति धारण किये हुए मनुष्य सोचता है कि वह जीवन के त्रिविध लक्ष्य तो प्राप्त कर ही रहा है और ऐसा सोच कर वह उनमें आसक्त हो जाता है। वह अपने कृत्यों का परिणाम चाहता है। वह धर्म, काम और अर्थ के लिए संघर्ष करता है। ऐसे मनुष्य की धृति राजसिक अभिहित है। हे अर्जुन, अब तीसरे प्रकार की धृति तामसी धृति के विषय में सुनो।
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ।। ३५ ।।
शब्दार्थ : यया-जिसके द्वारा, स्वप्नम् -निद्रा, भयम् -भय, शोकम् - शोक, विषादम् अवसाद, निराशा, मदम्-उन्मत्तता, एव-ही, च-और, ने-नहीं, विमुञ्चति-त्यागता, दुर्मेधा मूर्ख, धृतिः- धृति, सा-वह, पार्थ-हे पार्थ, तामसी-तामसिक ।
अनुवाद : हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा अविवेकी मनुष्य, निद्रा, भय, शोक, अवसाद और मद का त्याग नहीं करता, वह धृति तामसिक है।
व्याख्या : अविद्या रूपी अन्धकार का मूर्तिमान् मनुष्य, प्रत्येक सम्भव दुर्गुण से निर्मित है। वह अत्यन्त तंद्रिल और पापी है। वह असामान्य रूप से ही निद्रा प्रसक्त रहता है। वह विषय सेवन को ही उपयुक्त मानता है। अशुभ कर्मों के कारण वह दुःख का भोगी भी बनता है। अत्यन्त आत्माभिमानी (देह में आसक्त) होने के कारण वह सदा भयग्रस्त रहता है। सन्तुष्ट तो कभी वह होता ही नहीं। वह कामी और आत्म प्रवंचक होता है। वह आचार-व्यवहार नहीं जानता। वह क्रोधी और उद्धत (उन्मत्त) होता है। वह इन्द्रिय-विषयों में सुख का अनुभव करता है।
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।। ३६ ।।
शब्दार्थ : सुखम् -सुख, तु-निश्चित रूप से, इदानीम् - अब, त्रिविधम्-तीन प्रकार का, शृणु सुनो, मे—मुझ से, भरतर्षभ - हे भरत श्रेष्ठ, अभ्यासात् अभ्यास से, रमते-सुखी होता है, यत्र-जिसमें, दुःखान्तम् दुःख का अन्त, च-और, निगच्छति -प्राप्त करता है।
अनुवाद : हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मुझ से तीन प्रकार के सुख को सुनो (सुनने के लिए चित्त को एकाग्र करो)। जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से अथवा पुनः पुनः उसकी आवृत्ति करने पर रमता है और निश्चित रूपेण वह दुःख की निवृत्ति करने वाला है।
व्याख्या : आत्मा द्वारा आनन्द की अल्पानुभूति सब दुःखों को विराम दे सकती है। यह सुख अथवा आनन्द भी तीन प्रकार का है। हे अर्जुन, अब मैं उन के विषय में पृथक् रूप से उपदेश करूँगा। (निरूपण- VI.20.30)
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ।। ३७ ।।
शब्दार्थ : यत्-जो, तत्वह, अग्रे आरम्भ में, विषम् - विष, इव-समान, परिणामे अन्त में, अमृतोपमम्-अमृत के समान, तत्-वह, सुखम् -सुख, सात्त्विकम् -सात्त्विक, प्रोक्तम् -कहा गया आत्मबुद्धिप्रसादजम् - आत्म बुद्धि के प्रसाद (शुद्ध मन) से उत्पन्न । है,
अनुवाद : आरम्भ में विष के समान और परिणाम (अन्त) में अमृत तुल्य-ऐसे सुख को विद्वानों ने सात्त्विक घोषित किया है क्योंकि यह आत्म बुद्धि के प्रसाद रूप निर्मल मन से उत्पन्न हुआ है।
व्याख्या : अग्रे विषमिव-आरम्भ में यह अत्यन्त श्रम साध्य होता है क्योंकि कठोर साधना और कठिन तपश्चर्या के लिए विश्राम और विषय-वासनाओं का त्याग करना पड़ता है। यम, नियम, तपस् एवम् अन्य व्रतों का अभ्यास करने के लिए साधक को अत्यन्त कठिन परीक्षा से साक्षात्कार करना पड़ता है। उसे इन्द्रिय-विषयों से वैराग्य और अनासक्ति का विकास करना होता है। प्रारम्भ में यह अत्यन्त कष्ट साध्य प्रतीत होता है। एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास भी प्रारम्भ में दुःखद प्रतीत होता है। इन्द्रियों का वशीकरण अतीव क्लिष्ट है। वरस्वरा औषधि (Nux Vomica) प्रारम्भ में अति कटु लगती है। इसका मिश्रण लेने पर मनुष्य पहले तो बहुत पीड़ा अनुभव करता है किन्तु अन्त में उसे सुखद् अनुभूति होती है जब वह शक्ति प्राप्त करता है, उसकी पाचन शक्ति बढ़ती है और मन्दाग्नि ठीक हो जाती है। एवंविध, साधक अमरता का अमृतपान अन्त में करता है, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति करता है, उसका अन्तःकरण पूर्ण सन्तोष को प्राप्त करता है और वह परम शान्ति और शाश्वत आनन्द में रहने लगता है।
प्रोक्तम् - विद्वानों द्वारा कथित ।
आत्मबुद्धिप्रसादजम् – (अपनी ही) आत्म बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न अथवा ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान से उद्भूत। वह ब्रह्म जो अविनाशी है, स्वयं प्रकाश है, शाश्वत है, परमात्मा है और सर्वस्व है। उस सर्वोच्च आत्म तत्त्व से तादात्म्यता स्थापित कर के जीवात्मा सात्त्विक सुख का आनन्द लेता है।
इस प्रकार से उद्भूत सुख सात्त्विक है। (निरूपण - VI.1.2.)
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे ऽमृतोपमम् ।
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ।।३८ ।।
शब्दार्थ : विषयेन्द्रियसंयोगात् - इन्द्रियों का विषयों के साथ संयोग, यत्-जो, तत्वह, अग्रे-आरम्भ में, अमृतोपमम् - अमृत सदृश, परिणामे-अन्त में, विषम् - विष, इव-समान, तत्-वह, सुखम् -सुख, राजसम् राजसिक, स्मृतम् -कहा गया है।
अनुवाद : इन्द्रियों का विषयों के साथ संसर्ग होने से जो सुख मिलता है, वह प्रथम तो अमृत तुल्य प्रतीत होता है किन्तु अन्त में विष तुल्य होता है। ऐसा सुख राजसिक कहा है।
व्याख्या : इन्द्रिय सुख दुःख, भय और पाप से मिश्रित होता है। राई समान इन्द्रिय सुख अन्त में पर्वत समान दुःख में परिणत हो जाता है। ऐन्द्रिक सुख में आसक्त रहने वाले व्यक्ति को साथ ही साथ दुःख का सामना भी करना पड़ता है। उसे प्राप्त विषयों के विनाश का भय सताता है क्यों कि वह उनमें आसक्त है। आसक्ति मृत्यु है। यह व्यक्ति को पुनः पुनः इस मर्त्य लोक में ले आती है। आसक्ति और भय इन्द्रिय विषयों के सहचर हैं। धन प्राप्ति हेतु उसे संघर्ष करना पड़ता है। धन से वह सुख के विषयों का क्रय कर सकता है। संघर्ष की अवधि में वह अनेक पाप कर्म करता है जिसका परिणाम उसे नरक में भोगना पड़ेगा। अगला जन्म अत्यन्त निम्न श्रेणी में होगा। धन के लिए वह मिथ्या भाषण और कपट करता है। इन्द्रियाँ भी वासना युक्त हो कर शक्ति हास कर बैठती हैं। व्यक्ति अपनी शक्ति, बल, धन, ऊर्जा का विनाश कर लेता है। उसकी बुद्धि क्षीण, दुर्बल, मूढ़, अपवित्र और विपरीत हो जाती है। वह धन और विवेक खो देता है। (निरूपण - V.22)
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ।।३९ ।।
शब्दार्थ : यत्-जो, अग्रे-आरम्भ में, च-और, अनुबन्धे-परिणाम में, च-और, सुखम् -सुख, मोहनम् - मोहित करने वाला, आत्मनः-अपना, निद्रालस्यप्रमादोत्थम् -निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न, तत्-वह, तामसम् - तामसिक, उदाहृतम् -कहलाता है।
अनुवाद : जो सुख प्रारम्भ में और अन्त में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है और निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वह तामसिक कहा जाता है।
व्याख्या : अनुबन्धे-परिणाम में, उपभोग के उपरान्त । बुरी आदतों से प्राप्त होने वाला सुख जैसे मदिरापान और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन-ये आत्मा को मोह में डालने वाले होते हैं। मनुष्य अपने सत् पथ से च्युत हो जाता है जिस पथ से उसे चलना चाहिए था । निस्सन्देह ऐसा सुख तामसिक प्रकृति का कहा जाता है।
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ||४० ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, तत्-वह, अस्ति-है, पृथिव्याम् - पृथिवी पर, वा-अथवा, दिविदेव लोक में, देवेषु-देवताओं में, वा अथवा, पुनः पुनः, सत्त्वम् - प्राणी, प्रकृतिजैः -प्रकृति से उत्पन्न, मुक्तम्-मुक्त, यत्-जो, एभिः- इनसे, स्यात् -हो, त्रिभिः-तीन से, गुणैः- गुणों से।
अनुवाद : भूलोक में अथवा स्वर्ग लोक में देवताओं में भी ऐसा कोई प्राणी अथवा वस्तु नहीं है जो प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो।
व्याख्या : वस्त्र में धागे की भाँति गुण प्रत्येक वस्तु में ताने-बाने की भाँति विद्यमान हैं, ग्रथित हैं।
मनुष्यों का भूलोक हो अथवा देवों का द्युलोक हो-इह लोक और परलोक में कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के इन तीन गुणों से बंधा हुआ न हो। धागे के बिना क्या वस्त्र के अस्तित्व की कल्पना हो सकती है? अस्थि और रुधिर के बिना क्या मानव संरचना की कल्पना हो सकती है? पत्थर के बिना क्या कोई पर्वत हो सकता है? इसी प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसकी रचना में तीन गुण प्रवेश नहीं पाते। सम्पूर्ण सृष्टि इन्हीं तीन गुणों की कारीगरी है। इन गुणों ने त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) को प्रकट किया। इस मर्त्य लोक में कर्ता, कर्म और फल का त्रैगुण्य (त्रैविध्य) इन तीन गुणों से उद्भूत है। वे ही चार वर्णाश्रमों के विविध कर्मों का कारण हैं। इस संसार की उपमा अध्याय (XV.1) में पीपल के वृक्ष से दी गई है। इस संसार की रचना तीन गुणों से हुई है और गति अविद्या की शक्ति से हो रही है।
कर्म, कर्म का उपादान कारण और फल-इन तीन से संसार गतिशील है और यह चक्र अनादिकाल से घूम रहा है। केवल मुक्त संन्यासी ही, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, इस चक्र की गति को विराम देता है, कारण और कार्य से अतीत जा कर कर्म बन्धन की श्रृंखला को तोड़ देता है।
विरक्ति की अटूट खड्ग से संसार के इस रहस्यमय वृक्ष का उन्मूलन कर डालो। तीन गुणों से अतीत गमन कर के अपनी मूल दिव्य प्रकृति सत्-चित्-आनन्द में विश्राम करो।
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ।।४१ ।।
शब्दार्थ : ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् - ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के, शूद्राणाम् - शूद्रों के, च-और, परंतप - हे परंतप, कर्माणि कर्तव्य कर्म, प्रविभक्तानि विभाजित हैं, स्वभावप्रभवैः- उनकी अपनी प्रकृति से उत्पन्न, गुणैः गुणों से।
अनुवाद : हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म भी स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुरूप ही विभक्त किये गये हैं।
व्याख्या : ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को वेद-पाठ का अधिकार प्राप्त है। किन्तु हे अर्जुन, चतुर्थ श्रेणी के लोगों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है क्यों कि उनका कर्तव्य प्रथम तीन श्रेणी के लोगों की सेवा करना है। उन्हें वेद पढ़ने अथवा यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। मानव समुदाय चार जातियों में विभक्त है और प्रत्येक मानव के जीवन की चार अवस्थायें हैं जो उनके गुणों और विकास-स्तर पर आधारित हैं। अब मैं गुणों के अनुरूप इन जातियों के विशेष कर्तव्यों का उपदेश करूँगा जिससे वे स्वयं को जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त कर के आत्म-ज्ञान का आलोक प्राप्त कर सकें। किंचित् तमस् मिश्रित रजोगुण से वैश्य जाति का विकास होता है, जिनका प्रमुख कर्म व्यापार है। रजस् मिश्रित तमोगुण से शूद्र जाति का उद्भव होता है।
तीन गुणों पर आधारित एक मनुष्य जाति चार जातियों में विभक्त है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के आधार पर उनके कर्म निश्चित किये जाते हैं। प्रकृति (स्वभाव) ईश्वर की प्रकृति (माया) है जो सत्त्व, रजस् और तमस्, तीन गुणों से युक्त है।
ब्राह्मण की प्रकृति सात्विक होती है। अतः वह शान्त और सौम्य रहता है। क्षत्रिय की प्रकृति सत्त्व मिश्रित रजस् है। उसमें रजोगुण की अपेक्षा सत्त्व गौण होता है, रजस् प्रधान होता है। इसलिए वह प्रभुत्व का अधिकार रखता है। वैश्य की प्रकृति रजस् और तमस् है। इसमें तमस् गौण और रजस् प्रधान है। इसीलिए वह धन अर्जित करने के लिए विविध प्रकार की प्रक्रियायें करता है। शूद्र की प्रकृति तमस् है, उसमें रजस् गौण है। वह मूढ़ होता है।
कर्म-वह क्रिया जो पूर्व संस्कार और इच्छा के अनुरूप अभिव्यक्त होती है। बिना कारण के गुणों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। प्राणियों में स्वभाव उनकी वृत्ति, संस्कार और वासना के कारण है। पूर्व जन्मों में उन्होंने यह प्राप्त किया था। वर्तमान जन्म में यह स्वयं को अभिव्यक्त करता है और प्रभाव उत्पन्न करता है। यह प्रकृति गुणों का स्रोत है। प्रत्येक मनुष्य अथवा नारी अपने स्वभाव से उत्पन्न है। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों के अनुरूप गुण उसे अपने स्वाभाविक कार्य (परिणाम) के रूप में उसे अपना कर्तव्य कर्म करने को प्रेरित करते हैं। व्यक्ति विशेष के गुणों के अनुरूप ही चारों जातियों में कर्म विभाजित किये गये हैं। (निरूपण - IV.13)
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ।।४२ ।।
शब्दार्थ : शमः -प्रशान्ति, दमः - आत्म-निग्रह, तपः-तपस्या, शौचम् - पवित्रता, क्षान्तिः-क्षमा, आर्जवम् -सरलता, एव-ही, चऔर, ज्ञानम् - ज्ञान, विज्ञानम् - विज्ञान, आस्तिक्यम् - ब्रह्म में श्रद्धा, ब्रह्मकर्म-ब्राह्मण के कर्म हैं, स्वभावजम् -स्वभाव जन्य (अपने स्वभाव से उत्पन्न) ।
अनुवाद : शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जवता, ज्ञान, विज्ञान, और परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास- ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं।
व्याख्या : शम मन का निग्रह है। दम इन्द्रिय-निग्रह है। शम और दम की XVII.2 में व्याख्या हो चुकी है। तीन प्रकार का तप भी XVII.14.15.16 में बताया जा चुका है।
आस्तिक्यम् गुरु के वचनों में विश्वास, शास्त्रों के उपदेश में श्रद्धा, परमात्मा की सत्ता में विश्वास, इस जीवन के उपरान्त भी सत्ता में विश्वास और सर्वोपरि आत्म तत्त्व में विश्वास आस्तिक्य है।
मन आत्मा में विलीन होता है और शान्ति देता है। आत्म-नियंत्रण शान्ति में सहायक है। शास्त्रों के उपदेश का अनुपालन कर के तुम शान्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हो। अधिक तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। शिक्षा के प्रति सम्मान का भाव और श्रद्धा-विश्वास होना चाहिए।
जिस प्रकार चन्दन का वृक्ष अपनी ही मधुर सुगन्ध से सुगन्धित है, चम्पक वृक्ष अपने ही सुन्दर प्रिय पुष्पों से विभूषित है उसी प्रकार एक ब्राह्मण भी इन नौ गुणों से विभूषित है जो उससे पृथक् नहीं किये जा सकते।
हे अर्जुन, अब क्षत्रिय के कर्तव्य सुनो :
शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ।।४३ ।।
शब्दार्थ : शौर्यम् - शूरवीरता, तेजः-तेज, धृतिः दृढ़ता, संकल्प, धारणा, दाक्ष्यम् - चुतराई, युद्धे-युद्ध में, च-और, अपि-भी, अपलायनम् न भागना, दानम् दान, ईश्वरभावः नेतृत्व, प्रभुत्व (पीठ न दिखाना), च-और, क्षात्रम् - क्षत्रियों का, कर्म-कर्म, स्वभावजम् स्वाभाविक ।
अनुवाद : शूरवीरता, तेज, धारणा, दक्षता, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान और नेतृत्व-ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं।
क्षत्रिय (योद्धा अथवा राज पुरुष) का प्रथम कर्तव्य है कि वह शौर्यगुण और पौरुष से युक्त हो । शूरवीरता वह उत्कृष्ट गुण है जिसके द्वारा मनुष्य स्वभावतः ही बलशाली, सुविक्रान्त और साहसी होता है। अत्यधिक विपदा काल में भी उसका मन किंचिदपि विचलित नहीं होता। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्षत्रिय अडिग रहेगा। विपरीत दशाओं में भी अवसाद युक्त अथवा शोकाकुल नहीं होगा। यह कौशल है, दक्षता है जिसके द्वारा विचारणाशक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी मार्ग चयन कर के सहज ही लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है। यह धृति है, धारणा है, साहस है।
दक्ष्य-कुशलता । अनेक कार्यों में जहाँ कुशाग्र अवधारणा की आवश्यकता हो वहाँ वह सद्यः उचित निर्णय लेने में समर्थ होता है। ऐसे कर्तव्य कर्म जो अनायास ही समक्ष आ पड़ते हैं उन्हें बिना किसी प्रकार के भ्रम अथवा व्याकुलता से पूर्ण करना दक्षता है।
सूरजमुखी का पुष्प सदा सूर्य की ओर अपना मुख कर लेता है, ऐसे ही क्षत्रिय अपने शत्रु का सामना करता है।
युद्ध क्षेत्र में वह कभी पीठ नहीं दिखाता। वह सर्वथा निर्भय है। जिस प्रकार वृक्ष अपने फूल और फल इसकी इच्छा करने वाले को बहुलता में प्रदान करता है, चमेली अपनी मधुर सुगन्ध सब दिशाओं में प्रकीर्ण करती है इसी प्रकार क्षत्रिय, मांगने वाले को मुक्तहस्त से दान करता है। उसका दान असीम है।
नेतृत्व-एक क्षत्रिय राजा अपना विश्वस्त रक्षण देने के विश्वास से प्रजा पर राज्य करता है। शासन जिन पर किया जाना चाहिए उन पर शासन करता है और अधर्मी तथा दुराचारी जनों को दण्ड देने के लिए धर्म का 'दण्ड' धारण करता है।
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ।।४४ ।।
शब्दार्थ : कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यम् -कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य, वैश्यकर्म- वैश्य के कर्म, स्वभावजम् -स्वाभाविक, परिचर्यात्मकम् -सेवा रूप, कर्म-कर्म, शूद्रस्य-शूद्र के, अपि-भी, स्वभावजम् -स्वाभाविक ।
अनुवाद : कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं और सेवा आदि परिचर्यात्मक कर्म शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं।
व्याख्या : मनुष्य जब अपने कर्तव्य कर्म अपने वर्ण और जीवन की अवस्था के अनुसार समुचित प्रकार से करता है, उसका हृदय परिष्कृत हो जाता है और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अपस्तम्भ धर्मसूत्र में कहा गया है- "विभिन्न वर्गों और अवस्थाओं वाले मनुष्य मृत्यूपरान्त कर्मों का परिणाम प्राप्त करते हैं और अवशेष कर्मों के प्रभाव वश श्रेष्ठतर देश, वर्ण, परिवार में जन्म लेते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ धर्म, जीवन की अवधि, शिक्षा, चरित्र, सम्पत्ति, सुख और मेधा से युक्त होता है' '(२,२,२,३) । जीवन की चार अवस्थाओं और वर्ण व्यवस्था के अनुरूप मनुष्य द्वारा किये गये कर्मों और लोकों का वर्णन पुराणों में भी विस्तार से मिलता है।
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ।। ४५ ।।
शब्दार्थ : स्वे स्वे-अपने अपने, कर्मणि-कर्म में, अभिरतः संलग्न, को, लभते-प्राप्त करता है, नरः मनुष्य, संसिद्धिम् -सफलता स्वकर्मनिरतः - अपने कर्म में संलग्न, सिद्धिम् - सिद्धि को, यथा-जैसे, विन्दति-प्राप्त करता है, तत्-वह, शृणु-सुनो।
अनुवाद : अपने अपने कर्म में निरत प्रत्येक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। वह अधिकारिक कर्म निरत हो कर कैसे सिद्धि प्राप्त करता है, वह सुनो।
व्याख्या : यह श्रम का विभागीकरण है जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति और वर्ण के अनुरूप कार्यरत है। विहित कर्तव्य तुम्हारा एकमात्र अधिकार है और परमात्मा के प्रति सर्वोच्च सेवा यही है कि अपने कर्तव्य का अनन्य मन से पालन करो और समस्त कर्म परम देव को समर्पित करते हुए फल की आकाङ्क्षा मत करो। निश्चित रूप से तुम आध्यात्मिकता में प्रगति करोगे । कर्तव्य कर्म पूर्ण करने से तुम्हारा अन्तःकरण परिष्कृत हो जायेगा और तुम आत्म-ज्ञान के अधिकारी बन जाओगे।
स्वे स्वे कर्मणि-अपने वर्ण और गुण (प्रकृति) के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म में तत्पर। केवल कर्म करने से मोक्ष पाना तो असम्भव है किन्तु कर्म हृदय को परिमार्जित करता है और साधक को दिव्य ज्ञान ज्योति प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनाता है।
कर्म के लिए पूजा का भाव विहित है। अर्थात् कर्म ही पूजा है, ऐसा सोच कर तत्परता से अपने अपने कर्म में रुचि लेनी चाहिए।
यतः प्रवत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ।।४६ ।।
शब्दार्थ : यतः - जिससे, प्रवृत्तिः उत्पत्ति, भूतानाम् -प्राणियों की, येन-जिसके द्वारा, सर्वम्-सब, इदम् - यह, ततम्-व्याप्त, स्वकर्मणा-अपने कर्म से, तम् - उसे, अभ्यर्च्य पूजा करते हुए, सिद्धिम् -सिद्धि, विन्दति-प्राप्त करता है, मानवः मनुष्य ।
अनुवाद : जिससे समस्त प्राणियों का उद्भव हुआ है और जिससे यह सब व्याप्त है, अपने कर्म द्वारा, ईश्वर की आराधना कर के मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है।
व्याख्या : जिस परम पिता परमात्मा से इस जगत् की उत्पत्ति हुई है उसके संकल्प को कार्य रूप प्रदान करना ही मनुष्य के लिए स्व स्व कर्म का पालन करना है। अपने कर्तव्य कर्म रूप पुष्पों से मनुष्य जब उस परम पुरुष की पूजा करता है वह अत्यन्त प्रसन्न होता है और पूजा से सन्तुष्ट हो कर आराधक पर विवेक और वैराग्य के वरदान रूप में वृष्टि करता है।
प्रवृत्तिः-उद्भव अथवा चेष्टा । यह ईश्वर से प्रवृत्त होती है जो सब का अन्तर्यामी है।
स्वकर्मणा-अपने कर्म से, अपने वर्ण के अनुसार, जैसे ऊपर बताया गया है।
भूतानाम् - प्राणियों की।
अपना कर्म करते हुए मानो ईश्वर की पूजा करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है अर्थात् वह ज्ञान योग का अधिकारी बन जाता है।
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ।।४७ ।।
शब्दार्थ : श्रेयान् श्रेयस्कर, स्वधर्मः- अपना कर्तव्य कर्म, विगुणः गुण रहित, परधर्मात् -दूसरे के धर्म से, स्वनुष्ठितात्-भली प्रकार अनुष्ठान किये हुए, स्वभावनियतम् स्वभाव से नियत किया हुआ, कर्म-कर्म, कुर्वन् करते हुए, न-नहीं, आप्नोति-प्राप्त करता है, किल्बिषम् - पाप को।
अनुवाद : दूसरे के द्वारा भली प्रकार अनुष्ठान किये हुए धर्म की अपेक्षा अपना गुण रहित धर्म भी श्रेष्ठतर है। अपने स्वभावजन्य कर्म को करने वाला मनुष्य कभी पाप का अधिकारी नहीं बनता।
व्याख्या : जिस प्रकार विष में उत्पन्न होने वाले कीट के लिए विष हानिकर नहीं होता उसी प्रकार स्वभावजन्य कर्म (स्वधर्म) मनुष्य के लिए दोषयुक्त अथवा पाप कर्म नहीं होता।
संसार के लिए जो विष है, कीट के लिए वह मिठाई है पुनरपि ईख का मधुर रस उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है।
अतः मनुष्य को, नियत कर्म का पालन करना चाहिए जो कठिन तो है किन्तु उसे बन्धन मुक्त करने वाला होता है। दूसरे का कर्म भयावह होता है। अज्ञानी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। (निरूपण -III.35)
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ।।४८ ।।
शब्दार्थ : सहजम् - जन्म के साथ उत्पन्न, कर्म-कर्म, कौन्तेय-हे कौन्तेय, सदोषम् दोष युक्त, अपि-भी, न-नहीं, त्यजेत्-त्याग करें, सर्वारम्भाः समस्त कर्म, हि-क्योंकि, दोषेण-दोष से, धूमेन-धूम से, अग्नि -अग्नि , इव-भाँति, आवृताः- आच्छादित है।
अनुवाद : हे अर्जुन, सहज कर्म दोषयुक्त होते हुए भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि धूम से अग्नि की भाँति समस्त कर्म दोष से आवृत हैं।
व्याख्या : सहजम् - जन्म के साथ उत्पन्न ।
सदोषम् -दोष युक्त, क्योंकि प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है।
सर्वरम्भाः समस्त कर्म, अपने हों अथवा दूसरों के।
कोई वैश्य अथवा क्षत्रिय ब्राह्मण के कर्म करने लगे तो किसी प्रकार से भी वह उसके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। दूसरे का कर्म भय प्रदान करने वाला होता है। इसलिए दूसरे का कर्म करना निषिद्ध है। आत्म-ज्ञान के बिना अशेषेण कर्म त्याग किसी भी मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है। अतः कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।।४९ ।।
शब्दार्थ : असक्तबुद्धिः - जिसकी बुद्धि अनासक्त है, सर्वत्र-सर्वत्र, जितात्मा-जिसने अन्तःकरण को वश में कर लिया है, विगतस्पृहः- तृष्णा जिसकी नष्ट हो चुकी है, नैष्कर्म्यसिद्धिम् - निष्कर्मता रूप सिद्धि, कर्म के त्याग से होने वाली सिद्धि, परमाम् -परम, संन्यासेन संन्यास से, अधिगच्छति-प्राप्त करता है।
अनुवाद : जिसकी बुद्धि सर्वत्र सब विषयों में अनासक्त है, जिसने आत्म संयम प्राप्त कर लिया है, जो आप्तकाम है (जिसकी तृष्णायें समाप्त हो चुकी हैं), वह संन्यास द्वारा कर्म से मोक्ष की परमावस्था को प्राप्त होता है।
व्याख्या : जिस व्यक्ति का मन स्त्री, पुत्र, देह, सम्पत्ति में आसक्त नहीं है, जिसने मन और इन्द्रियों का निग्रह कर लिया है, जिसे अपने शरीर, जीवन अथवा विषय वासनाओं के लिए कोई इच्छा नहीं है, वह भगवतोन्मुख होता है। सांसारिक विषयों में वह आकृष्ट नहीं होता। वह विवेक और वैराग्य से युक्त होता है।
शनैः-शनैः वह सत्-चित्-आनन्द स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त कर लेता है ऐसा आत्मज्ञानी कर्म से संन्यास द्वारा सर्वोच्च सिद्धि, मोक्ष को प्राप्त करता है।
आत्म-ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। क्रिया को विराम मिलता है। सम्भव है व्यक्ति संसार की रुचि के लिए कर्म करे पुनरपि वह कर्म बन्धन में नहीं आता क्योंकि उसने आत्म-ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से कर्म से संन्यास ले लिया है। ज्ञानाग्नि ने कर्मों के फल लाने वाले प्रभाव को भस्म कर दिया है। कर्मों को ही निष्फल कर दिया है। अहंकार से मुक्त होने के कारण उसमें कर्तृत्व भाव का सर्वथा नाश हो गया है और वह परम पुरुष से एकरूप हो गया है।
नैष्कर्म्य सिद्धि-इसका अभिप्राय निष्कर्म्यता से भी हो सकता है। इस उत्कृष्ट, महिमान्वित, अनिर्वचनीय दिव्य आलोक की अवस्था में मनुष्य निष्क्रिय आत्मा के रूप में स्थित रहता है। यह वेदान्तियों की सद्यः मुक्ति अथवा कैवल्य मोक्ष की अवस्था है। आत्म-ज्ञान प्राप्त होने पर सम्यक् ज्ञान, संन्यास अथवा सर्वकर्म परित्याग से इस अलौकिक अवस्था की प्राप्ति होती है। "मनसा सर्वकर्म परित्याग और संयम द्वारा देही इस नौ द्वार की पुरी में, न तो स्वयं कर्म करता हुआ न दूसरों को कर्म में प्रेरित करता हुआ सुखपूर्वक अधिष्ठित रहता है।" (निरूपण-V.13)
अब अगले श्लोक में भगवान् उपदेश करते हैं कि मनुष्य उपर्लिखित श्लोक ४६ के अनुसार सिद्धि प्राप्त कर के भगवान् की सेवा में अपने कर्म समर्पित करता हुआ किस प्रकार कर्म से मुक्त हो सकता है। वह विवेक लाभ करता है, ध्यान का सतत अभ्यास करता है और निर्विकार ब्रह्म के ज्ञान में विश्राम लेता है। (निरूपण—III.4, 19)
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।।५० ।।
शब्दार्थ : सिद्धिम् -सिद्धि, प्राप्तः - प्राप्त कर के, यथा-जैसे, ब्रह्म-ब्रह्म, तथा-वैसे, आप्नोति -प्राप्त करता है, निबोध जानो, मे मुझ से, समासेन-संक्षेप में, एव-ही, कौन्तेय-हे कौन्तेय, निष्ठा-निष्ठा, अवस्था, ज्ञानस्य-ज्ञान का, या-अथवा, परा-सर्वोच्च ।
अनुवाद : हे अर्जुन, सिद्धि को प्राप्त हो कर अर्थात् कर्मों द्वारा ईश्वर की पूजा कर के मनुष्य किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है जो ज्ञान की चरम अवस्था है, वह तुम मुझ से संक्षेप में सुनो।
व्याख्या : गुरु से अध्यात्म का उपदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिलने पर मनुष्य का अहंभाव और द्वैतभाव विनाश को प्राप्त होता है और उसका मन परमात्मा की सन्निधि प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य को और कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके लिए करणीय कुछ भी शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य हो जाता है।
साधक ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है क्योंकि उसने अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की पूजा की है। भगवान् विरक्ति, विवेक और ज्ञान भक्ति का दान देते हैं। उसके अविद्या के आवरण को दूर करते हैं। “ऐसे सदा समन्वित रूप से आराधना करने वालों को मैं प्रेम करता हूँ। मैं उन्हें विवेक योग देता हूँ जिससे वे मेरे पास आते हैं। उनके प्रति अपनी अनुकम्पा मात्र से मैं उनकी आत्मा में वास करता हुआ ज्ञान के प्रकाश-दीप से उनका अविद्या रूपी अन्धकार मिटा देता हूँ।"
सिद्धि, ज्ञान में निष्ठा अथवा ज्ञान के प्रति भक्ति है जिसके द्वारा अविद्या का आवरण हटने पर मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है। भक्ति-ज्ञान योग प्राप्ति की विधि संक्षेप में, कम शब्दों में वर्णित की जायेगी। आत्म-ज्ञान की प्रक्रिया आगामी श्लोकों में संक्षेप में निरूपित की जायेगी। वास्तविक कला तो गुरु ही बता सकते हैं।
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्याऽऽत्मानं नियम्य च ।
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ।।५१ ।।
शब्दार्थ : बुद्धया-बुद्धि से, विशुद्धया-पवित्र, युक्तः- युक्त, धृत्या धृति से, आत्मानम्-अपने को, नियम्य-वश में कर के, च-और, शब्दादीन् शब्द आदि, विषयान् - विषयों को, त्यक्त्वा त्याग कर, रागद्वेषौ राग और द्वेष को, व्युदस्य-त्याग कर, चऔर।
अनुवाद : विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो कर, धारणा द्वारा आत्म-नियन्त्रण कर के, शब्दादि विषयों और राग-द्वेष का त्याग कर के,
व्याख्या : निम्न प्रकृति को परिष्कृत बुद्धि से संकल्प द्वारा संयत करना चाहिए। चंचल इन्द्रियों और मन को परिष्कृत बुद्धि अथवा विवेक से संयत करना चाहिए। विशुद्ध विवेक में महान् शक्ति है। जब भी इन्द्रियाँ अपना सिर उठायें, विवेक के शक्तिशाली दण्ड से उन पर आघात करना चाहिए। विवेक धृति की शक्ति है।
विशुद्ध बुद्धि-काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, संशय, मिथ्या अवधारणा से शून्य बुद्धि विशुद्ध है। यह निर्मल दर्पण के समान है। विशुद्ध बुद्धि ब्रह्म स्वरूप है। सहज ही यह ब्रह्मैक्य प्राप्त कर सकती है। विशुद्ध बुद्धि ब्रह्म में विलीन हो जाये तो प्रतिभासित बुद्धि (चिदाभास), जीव भी ब्रह्म में लीन हो जाता है। जीव ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाता है वैसे ही, जैसे घटाकाश, घट के टूटने पर महाकाश के साथ एकरूप हो जाता है।
आत्मानम् - शरीर और इन्द्रियों का समाहार (समुदाय) ।
प्रत्याहार और दम के अभ्यास से साधक इन्द्रियों को उन्हें सर्वस्व विषयों से विमुख करता है। धीरे-धीरे इन्द्रियाँ आत्मा में स्थित हो जाती हैं। उनकी बहिर्मुखी वृत्ति पूर्ण रूप से संयत हो जाती है। सतत ध्यान के अभ्यास के द्वारा साधक इन्द्रियों पर विजित होता है, अनासक्ति के अभ्यास से राग को जीत लेता है और पवित्र प्रेम, वैश्विक दिव्य प्रेम के द्वारा द्वेष पर विजय प्राप्त करता है।
वह सब ऐश्वर्यों का त्याग कर देता है। शरीर के निर्वाह हेतु अनिवार्य बस्तुओं को ही वह रखता है। उन आवश्यक पदार्थों के प्रति भी न तो उसे आसक्ति होती है और न घृणा का भाव ।
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ।।५२ ।।
शब्दार्थ : विविक्तसेवी-एकान्तवासी, लघ्वाशी-अल्पाहारी, यतवाक्कायमानसः-मन, वाणी और शरीर जिसके संयत हों, ध्यानयोगपरः- ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करने वाला, नित्यम् - नित्य, वैराग्यम्-वैराग्य, समुपाश्रितः - आश्रित ।
अनुवाद : एकान्त वास करता हुआ, अल्पाहार लेता हुआ, मन, वाणी और शरीर को वश में कर के ध्यान योग परायण हो कर सदा वैराग्य के आश्रित हो कर,
व्याख्या : एकान्त का अपना ही आनन्द है। एकान्तवास में आध्यात्मिक संवेदन अद्भुत रूप से उन्नयनकारी होते हैं। बिना प्रयास के ध्यान सहज ही लग जाता है। आत्म-ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषि-मुनि वर्षों पर्यन्त एकान्त देश में रहे। नदी तट, गुहा, सागर तट अथवा वन्य प्रदेश ध्यान के लिए उचित स्थान है। ईस्टर और क्रिसमस के अवकाश में तुम एकान्त प्रदेश की शांति का आनन्द ले सकते हो। गृहस्थियों के लिए वर्ष में पन्द्रह दिन अथवा एक मास के लिए एकान्त वास आवश्यक है। अवकाश काल में कोलकाता अथवा अन्य नगर में रह कर समय, शक्ति और धन को व्यर्थ करने से अच्छा है कि ऋषिकेश, उत्तरकाशी अथवा नैमिषारण्य आदि पावन तीर्थस्थलों में जा कर रहो और अनुष्ठान (विधिविधान सहित कठिन अभ्यास), जप आदि करो और अमृतत्व के अधिकारी बनो। एक बार एकान्त का आनन्द ले लो तो कभी भूलोगे नहीं। इस आनन्द को पुनः ग्रहण करने का तुम्हारा प्रयास प्रत्येक वर्ष हो । अधिक खाने वाला आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए सक्षम नहीं है। अधिक भोजन आलस्य का कारण है और तन्द्रा और गहन सुषुप्ति भी अधिक भोजन से होती है। रहने के लिए खाओ । सन्तुलित आहार लो। तुम्हारा शरीर हल्का रहेगा, मन सौम्य और शान्त रहेगा। ध्यानाभ्यास में तुम्हें सहायता मिलेगी। सप्ताह के लिए अथवा मास भर के लिए मौन व्रत धारण करो। प्रतिदिन दो घण्टे मौन रहने का व्रत लो। शरीर को संयत रखो। अहिंसा और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो। आत्मा पर ध्यान एकाग्रित करो अथवा चतुर्भुज भगवान् विष्णु अथवा भगवान् कृष्ण अथवा राम अथवा शिव पर ध्यान लगाओ। ध्यान में नियमित रहो और धीरे-धीरे ध्यान की अवधि १५ मिनट से ३ से ६ घण्टे तक बढ़ाओ । पूर्ण समय के साधक हो तो पूर्ण समय ध्यान में लगाओ। ऐसा करने में समर्थ नहीं हो तो लिखित जप और कीर्तन करो। मध्यावकाश में धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करो। उन्नत उत्कृष्ट साधक ही दीर्घावधि तक ध्यानस्थ हो सकते हैं। मन का निरीक्षण करो और वैराग्य वृत्ति का विकास करो।
जागरूक न रहे तो इन्द्रियों के द्वारों से ऊर्जा क्षीण होने लगेगी। ऊर्जा क्षरण होने पर अच्छा ध्यान नहीं हो सकता। इहलोक और परलोक में इन्द्रिय- विषयों के प्रति उदासीनता वैराग्य है-विषय चाहे दृश्य हों अथवा अदृश्य, उनके प्रति उदासीनता और इच्छा का अभाव अनिवार्य है। वैराग्य स्थिर, प्रत्युत् चिरस्थायी होना चाहिए। यह क्षीण नहीं होना चाहिए। यह मन का अनवरत स्वभाव बन जाना चाहिए। पूर्णरूपेण वैराग्य में अधिष्ठित हो जाओ।
चालीस दिन के अनुष्ठान के लिए दूध और फल अथवा हल्का भोजन लो। केवल ३ अथवा ४ वस्तुएँ भोजन में लो। एक ही बार भोजन करो। धरती पर शयन करो। ब्रह्मचर्य और मौन व्रत धारण करो। कक्ष से बाहर मत आओ। पूर्ण मौन न रख सको तो अल्प भाषण करो। किसी पावन नदी अथवा गङ्गा तीर पर अनुष्ठान करो। अपने इष्ट मन्त्र के एक अथवा अनेक पुरश्चरण कर डालो। मन्त्र में यदि पाँच वर्ण हैं तो पाँच लाख बार मन्त्र की पुनरावृत्ति एक पुरश्चरण पूर्ण करेगी।
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।५३ ।।
शब्दार्थ : अहंकारम् - मिथ्या अभिमान, बलम्-बल, दर्पम् गर्व, कामम् - इच्छा, क्रोधम् -क्रोध, परिग्रहम् -दूसरे के धन का लालच, विमुच्य-त्याग कर, निर्ममः-अनासक्त, 'मेरा' भाव से रहित, शान्तः शान्त, ब्रह्मभूयाय-ब्रह्मभाव के लिए, कल्पते-योग्य है।
अनुवाद : अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह और "ममत्व" की भावना का त्याग करने वाला और शान्त चित्त वाला ब्रह्मरूप होने के योग्य हो जाता है।
व्याख्या : अहंकार -शरीर में आत्मा का अध्यास । यह शरीर को ही आत्मा मानने की भूल है।
बलम् वह बल अथवा शक्ति जो आसक्ति, इच्छा और मोह से संयुक्त है, यह शारीरिक शक्ति के लिए नहीं है प्रत्युत् शारीरिक शक्ति तो स्वाभाविक हुआ करती है जिसका आप त्याग नहीं कर सकते ।
दर्पम् -गर्व, धृष्टता, आत्माभिमान, राजसिक प्रचंडता जिसके कारण मनुष्य स्वयं को बहुत महान् समझने लगता है। अधिक ज्ञान और धन का गर्व हो जाता है। दर्प आने पर मनुष्य धर्म का अतिक्रमण करता है और दुष्ट कार्य करने लगता है।
साधक तो शरीर के लिए अनिवार्य पदार्थों का भी त्याग कर देता है। वह परमहंस, परिव्राजक अथवा भ्रमणशील संन्यासी बन जाता है। उसे देह में आसक्ति नहीं रहती। वह जानता है कि यह शरीर भी अपना नहीं है।
शान्त-सौम्य, उपरति युक्त, शान्त ।
ऐसा साधक जो आत्म-ज्ञान में रत है, ज्ञान निष्ठ यति है, वह ब्रह्म रूप होने के योग्य है।
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ।।५४ ।।
शब्दार्थ : ब्रह्मभूतः ब्रह्म से तादात्म्यता प्राप्त करके, प्रसन्नात्मा -प्रमुदित मनुष्य, न-नहीं, शोचति-शोक करता है, न-नहीं, काङ्क्षति-इच्छा करता है, समः-सम, सर्वेषु सब में, भूतेषु प्राणियों में, मद्भक्तिम् -मेरी भक्ति को, लभते-प्राप्त करता है, पराम्परम।
अनुवाद : ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य प्रमुदित (प्रसन्न) रहता है। वह न तो शोक करता है और न ही कोई इच्छा करता है। वह समस्त प्राणियों में समभाव रखता है। ऐसा ज्ञानी मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है।
व्याख्या : ब्रह्मभूतः-ब्रह्मभाव को प्राप्त हो कर । ब्रह्म के साथ तादात्म्यता और मोक्ष की अवस्था का वर्णन अगले श्लोक में किया जायेगा।
वह प्रशान्त मन रहता है। वह युक्त और समन्वित रहता है। तुच्छ व्यक्तित्व का कुछ भी शेष नहीं रहता जो उसमें शोक या इच्छा उत्पन्न करे। यह अवस्था प्राप्त होने पर विषयों की अनेकता धीरे-धीरे अदृश्य हो जाती है और वह सर्वत्र एकत्व के दर्शन करता है। जाग्रत और स्वप्नावस्था की चेतना जो मिथ्या ज्ञान का कारण है, धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है।
शारीरिक अभावों के लिए वह शोक नहीं करता। अभाव पूर्ति में समर्थ न हो तब भी वह व्याकुल नहीं होता। सफलता, असफलता में वह मन का सन्तुलन बनाये रखता है। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए उसे कोई आकाङ्क्षा नहीं होती।
न शोचति न काङ्क्षति-न शोक करता है न प्रमुदित होता है।
'समं सर्वेषु भूतेषु' का अभिप्राय यह भी हो सकता है कि वह स्वयं को दूसरों के स्थान पर रखता है और उनके लिए भावना भी रखता है। यदि कोई अत्यन्त शोक अथवा अवसाद की अवस्था में होगा तो उसे भी वही अनुभव होगा। उसका हृदय अत्यन्त कोमल होता है। वह अत्यन्त दयालु स्वभाव का होता है। वह समस्त प्राणियों के सुख-दुःख को अपना ही सुख-दुःख मानता है। दूसरों की प्रसन्नता में वह प्रसन्न होता है और दूसरों के दुःख में दुःखी होता है। उसका हृदय इतना उदार होता है कि वह सब के लिए सुख-दुःख अनुभव करता है। मनुष्य को मनुष्य से पृथक् करने वाले अवगुण-ईर्ष्या, हृदय की संकुचितता, तुच्छ भावना, पृथकत्व, सब प्रकार के द्वेष और किसी के लिए अरुचि आदि की भावनाओं के प्रतिबन्धक उसमें पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। वह वैश्विक प्रेम से युक्त होता है। वह विश्व का कल्याण चाहने वाला हो जाता है। वह सब का मित्र बन जाता है। उदारशीलता की अवस्था का वर्णन शब्दातीत है। इसकी अनुभूति स्वयं ही करनी अपेक्षित है। ऐसा साधक मेरे प्रति अपार भक्ति भाव रखता है। अध्याय VII के श्लोक १६ में निर्दिष्ट सर्वोच्च भक्ति अर्थात् ज्ञानी की ज्ञान के प्रति भक्ति उसे प्राप्त होती है। (निरूपण-II.70)
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ।।५५ ।।
शब्दार्थ : भक्त्या-भक्ति से, माम् - मुझ को, अभिजानाति जानता है, जावान् -जितना, यः जो, च-और, अस्मि (मैं) हूँ, तत्वतः तत्व से, ततः तब, माम् -मुझे, तत्त्वतः वास्तव में, ज्ञात्वा-जान कर, विशते-प्रवेश करता है, तत्-उस, अनन्तरम् तत्पश्चात् ।
अनुवाद : भक्ति के द्वारा वह मुझे तत्त्व से जान लेता है कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। तब मुझे इस प्रकार तत्त्व से जान कर वह मुझ में ही प्रवेश कर जाता है।
व्याख्या : हे अर्जुन, मुझसे एकाकार हुआ भक्त निश्चय से मेरी ही आत्मा है, जिसने अनन्यमनस्क हो कर मेरी भक्ति की है। भक्ति, ज्ञान में पराकाष्ठा को पहुँचती है। दो से प्रारम्भ हो कर भक्ति अद्वैत में समाप्त होती है। परा भक्ति और ज्ञान एक हैं। भक्ति माता है, ज्ञान पुत्र है। भक्ति से ही वह जानता है कि मैं सर्वव्याप्त शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। वह जान जाता है कि मैं अद्वैत हूँ, अजन्मा, अव्यय, कारणरहित, स्वयंप्रभा, अखण्ड, अविकारी हूँ। वह जानता है कि सीमित प्रतिबन्धों के सब भेदों से मैं पृथक् हूँ। वह जानता है कि मैं अवलम्ब, स्रोत, गर्भ, आधार, प्रत्येक वस्तु का आश्रय हूँ। वह जानता है कि मैं सब प्राणियों का नियन्ता हूँ, मैं परम पुरुष हूँ, मायापति हूँ और यह संसार मात्र एक आभास है। इस प्रकार मुझे तत्त्व से जान कर ज्ञान प्राप्ति के उपरान्त वह मुझ में प्रवेश करता है।
' ज्ञान और प्रवेश' ये दो पृथक् क्रियायें नहीं हैं। जानना ही होना है। जानने का अभिप्राय है-आत्म-ज्ञान होना। किसी वस्तु के ज्ञान का अभिप्राय है वही हो जाना। प्रवेश ज्ञान प्राप्ति है। ये सब शब्दों के खेल हैं। ज्ञान और प्रवेश पर्यायवाची हैं। भावातीत आध्यात्मिक तत्त्वों की अवधारणा दुज्ञेय है। गुरुजन विभिन्न प्रकार के तथ्य, गूढार्थ, उपमा, दृष्टान्त, कथानक आदि से साधक को उस परम तत्त्व का ज्ञान कराने और स्पष्ट रूप से उसे ग्रहण कराने का प्रयास करते हैं। शब्द दोषयुक्त हैं। भाषायें भी दोषरहित नहीं हैं। वे आध्यात्मिक अनुभूतियों को पूर्णरूप से अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं। येन केन प्रकारेण गुरु, शिष्य साधक को यह आध्यात्मिक विचार प्रदान करने का प्रयास करते हैं।
आत्म साक्षात्कार तो शिष्य को ही करना होगा। जो निहितार्थ, उपमा, दृष्टान्त अथवा शब्दों के रूप में अभिव्यक्ति से परे है। उस अद्वैत ब्रह्म की उपमा कैसे दी जा सकती है? ये शब्द एक प्रकार से साधकों को प्रारम्भ में आध्यात्मिक तत्व का अवगाहन करने में सहायक मात्र हो सकते हैं। आत्म-ज्ञान के उपरान्त इन शब्दों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वह स्वयं ही ज्ञान का मूर्तरूप हो जाता है।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः ।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ।।५६ ।।
शब्दार्थ : सर्वकर्माणि-समस्त कर्म, अपि-भी, सदा-सदा, कुर्वाण:- करते हुए, मद्यपाश्रयः- मेरे आश्रित हो कर, मत्प्रसादात्-मेरी कृपा से, अवाप्नोति-प्राप्त करता है, शाश्वतम् - शाश्वत, पदम् -पद, धाम, अव्ययम् - अनश्वर ।
अनुवाद : सर्वदा मेरे आश्रित हो कर सब कर्म करते हुए, मेरे अनुग्रह से वह शाश्वत, अविनाशी पद को प्राप्त करता है।
व्याख्या : शुभ कर्मों के प्रसूनों से मेरी आराधना कर के वह मेरी अनुकम्पा से अक्षय्य तेज युक्त अविनाशी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। मेरे साथ एकत्व पा कर वह परम आनन्द का भोग करता है। यदि किसी अवसर पर वह निषिद्ध कर्म भी करता है तो उसके प्रभाव से वैसे ही अप्रभावित रहता है जैसे गङ्गा में नाले का पानी मिलने पर भी गङ्गा जल अप्रभावित रहता है।
ईश्वर की पूजा यदि अपने कर्तव्य-कर्मों द्वारा की जाये तो साधक का हृदय परिष्कृत होता है और उसकी ज्ञान-निष्ठा का विकास होता है जो अनायास ही उसे ज्ञान प्राप्ति की ओर उन्नत करती है। यहाँ भक्तियोग की श्लाघा की गई है।
सर्वकर्म-शुभ कर्म तथा निषिद्ध कर्म । मुझ वासुदेव भगवान् को सर्वस्व अर्पण कर देने वाला भक्त विष्णु के शाश्वत धाम को मेरे अनुग्रह से प्राप्त करता है।
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ।।५७ ।।
शब्दार्थ : चेतसा -विवेक बुद्धि से, सर्वकर्माणि-सब कर्म, मयि-मुझ में, संन्यस्य-अर्पण कर के, मत्परः- मेरे परायण, बुद्धियोगम् - योग (स्थिर बुद्धि) का, उपाश्रित्य-आश्रय लेकर, मच्चित्तः- मुझ में चित्त लगाकर, सततम् -सदा, भवरहो ।
अनुवाद : विवेक बुद्धि से सब कर्म मुझे समर्पित कर के, मुझे ही सर्वोच्च लक्ष्य मान कर, बुद्धि योग का आश्रय ले कर तुम अपना मन सदा मुझ में स्थिर करो।
व्याख्या : हे अर्जुन, विवेक बुद्धि पर अपना चित्त स्थिर कर के अपने समस्त कर्म मुझे समर्पित कर दो। तब उस विवेक बुद्धि के द्वारा तुम अपने आत्मा को शरीर से और चेष्टा से पृथक् देखोगे जो मेरे शुद्ध अस्तित्व में निवसित होगा।
चेतसा-चित्त से। ज्ञान निष्ठा से। वह ज्ञान जो मोक्षप्रद है और जिसकी प्राप्ति भगवान् को समर्पित निष्काम कर्म के द्वारा हृदय पवित्र होने पर होती है।
सर्वकर्माणि-सब कर्म, जो दृश्यादृश्य प्रभाव देने वाले हैं।
मयि-मुझ में।
अध्याय IX.27. में उपदेश किया गया है-तुम जो भी कर्म करो, जो भी भोजन करो आदि सब मुझे समर्पित करो।
मत्परः- मेरे परायण। मुझे ही परम लक्ष्य और आश्रय मान कर।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य-अनन्य-आश्रय, बुद्धि योग ।
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि ।।५८ ।।
शब्दार्थ : मच्चित्तः-अपना मन मुझ में स्थिर कर के, सर्वदुर्गाणि-सब बाधायें, मत्प्रसादात् -मेरे अनुग्रह से, तरिष्यसि-पार कर जाओगे, अथ-अब, चेत् यदि, त्वम्-तुम, अहंकारात्-अहंकारवश, न-नहीं, श्रोष्यसि -सुनोगे, विनक्ष्यसि नष्ट हो जाओगे।
अनुवाद : मुझ में अपना चित्त स्थिर कर के, मेरी कृपा से तुम सब बाधाओं को पार कर जाओगे और यदि अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे।
व्याख्या : हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन एकाग्र हो कर मुझ में स्थिर होगा तब तुम मेरी अनुकम्पा से सब कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर जाओगे। और यदि तुम मेरी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करोगे और अभिमान वश उनका निरादर करोगे तो नष्ट हो जाओगे।
दुर्गाणि बाधायें, कठिनाइयाँ, पाश गर्त (गड्ढा), प्रलोभन आदि ये सब आध्यात्मिक पथ की रुकावटें हैं और संसार की विविध प्रकार की कठिनाइयाँ भी इस पथ पर आरूढ़ व्यक्ति को सहनी पड़ती हैं।
अहंकार-यह विचार कि तुम शिक्षित हो। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए- "मैं स्वतन्त्र हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं बुद्धिमान् व्यक्ति हूँ। मैं दूसरों की सलाह क्यों लूँ?"
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।।५९ ।।
शब्दार्थ : यत् - यदि, अहंकारम्-अहंकार को, आश्रित्य-आश्रित हो कर, न-नहीं, योत्स्ये-युद्ध करूँगा, इति-इस प्रकार, मन्यसे मानते हो, मिथ्या-व्यर्थ, एषः यह, व्यवसायः-संकल्प, ते तुम्हारा, प्रकृतिः-स्वभाव, त्वाम् - तुम्हें, नियोक्ष्यति - नियोजित करेगी, प्रेरित करेगी।
अनुवाद : अहंकारवश यदि तुम सोचते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा यह संकल्प व्यर्थ है क्यों कि प्रकृति तुम्हें (युद्ध के लिए) प्रेरित करेगी।
व्याख्या : मन का यह दृढ़ संकल्प तुम्हारी अपनी ही आन्तरिक प्रकृति द्वारा व्यर्थ कर दिया जायेगा क्योंकि तुम्हारी प्रकृति तुम्हें प्रेरित करेगी, योद्धा के रूप में तुम्हें लड़ने के लिए उत्साहित करेगी, विवश करेगी। यह तो केवल भ्रम मात्र है कि तुम अर्जुन हो, ये लोग तुम्हारे सम्बन्धी हैं और इन्हें मार कर तुम पाप के अधिकारी बनोगे ।
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ।। ६० ।।
शब्दार्थ : स्वभावजेन-स्वभाव से उत्पन्न, कौन्तेय-हे कुन्ती पुत्र, निबद्धः बंधा हुआ, स्वेन-अपने, कर्मणा-कर्म से, कर्तुम् -करने के लिए, न-नहीं, इच्छसि चाहते हो, यत्-जो, मोहात्-मोहवश, करिष्यसि करोगे, अवशः-विवश हो कर, अपि-भी, तत्-वह।
अनुवाद : अपने स्वभाव से उत्पन्न अपने कर्म में बंध कर तुम विवश हो कर वह कर्म करोगे जो अब तुम मोह वश करना नहीं चाहते।
व्याख्या : हे अर्जुन, तुम एक योद्धा के बल, पराक्रम, वीर्य और कौशल से युक्त हो । अपनी प्रकृति के तुम आधीन हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारी प्रकृति तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त करेगी।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।।६१ ।।
शब्दार्थ : ईश्वरः ईश्वर, सर्वभूतानाम् -सब प्राणियों के, हृद्देशे-हृदय में, अर्जुन-हे अर्जुन, तिष्ठति-वास करता है, भ्रामयन्- घुमाते हुए, सर्वभूतानि-सब प्राणियों को, यन्त्रारूढानि-यन्त्र पर आरूद, मायया-माया के द्वारा।
अनुवाद : हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और शरीर रूपी यन्त्र पर आरूढ़ इन प्राणियों को अपनी माया की शक्ति से उनके कर्मानुसार भ्रमाता है।
ईश्वरः- संसार का नियन्ता, नारायण।
ईश्वर सब प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से स्थित है। शरीर रूपी यह अद्भुत यन्त्र उसी ने प्रदान किया है। उसी की ही शक्ति से सब प्राणी गतिशील हैं। ईश्वर तो वास्तव में हमारे अन्तःकरण का सच्चा नायक है।
मायया-भ्रम उत्पन्न कर के।
यन्त्रारूढ़ कठपुतलियों की भाँति ईश्वर सब प्राणियों को घुमा रहे हैं। (निरूपण - X.20; XIII.18)
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ।। ६२ ।।
शब्दार्थ : तम् उसकी, एव-ही, शरणं गच्छ शरण में जाओ, सर्वभावेन-पूर्ण भाव से, भारत- हे भारत, तत्प्रसादात्-उसकी कृपा से, पराम् -परम, शान्तिम्-शान्ति को, स्थानम् - धाम को, प्राप्स्यसि-प्राप्त करोगे, शाश्वतम् - नित्य ।
अनुवाद : हे अर्जुन, तुम पूर्ण भाव से (अपने सम्पूर्ण अस्तित्व से) उसी की शरण में जाओ। उस प्रभु की अहेतुकी कृपा से तुम परम शान्ति और शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे।
व्याख्या : ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। इच्छाओं को गुप्त मत रखो कि तुम उनकी मौन सन्तुष्टि कर लोगे । इच्छा और अहंकार आत्म समर्पण के मार्ग में दो महान् बाधायें हैं। क्रूरतापूर्वक उन्हें मार डालो।
संसार चक्र के दुःखों, कष्टों, बाधाओं से मुक्त होने के लिए अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ ईश्वर की ओर दौड़ पड़ो। ईश्वर को ही अपना एक आश्रय मानो । तब उसकी कृपा से तुम परम शान्ति और नित्य परम धाम प्राप्त करोगे ।
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।। ६३ ।।
शब्दार्थ : इति-इस प्रकार, ते तुम्हारे लिए, ज्ञानम् - ज्ञान, आख्यातम् -कहा गया है, गुह्यात् - गुह्य से भी, गुह्यतरम्-गुह्यतर, मया-मेरे द्वारा, विमृश्य-विचार कर के, एतत्-यह, अशेषेण-पूर्णतया, यथा-जिस प्रकार, इच्छसि इच्छा करते हो, तथा-वैसा, कुरु-करो।
अनुवाद : इस प्रकार गुह्य से गुह्यतर अत्यन्त रहस्यपूर्ण गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। इस पर पूर्णतया अच्छी प्रकार विचार कर के जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसा करो।
व्याख्या : किसी भी प्रकार के रहस्य से अतीत, गोपनीय रहस्य मैंने तुम्हें बता दिये हैं। यह उपदेश, वेदों का सार, गीता नाम से अभिहित है। यदि कोई इसका अनुसरण करता है और इसके भाव में जीवन जीता है तो वह निश्चित रूप से परम शान्ति, सर्वोच्च ज्ञान और अमृतत्व की प्राप्ति करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं। हे अर्जुन, इस गुप्त कोष का रहस्य मैंने तुम्हारे समक्ष प्रकट कर दिया है क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो।
एतत् यह अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट उपदेश । तुम्हें जो भी उपदेश दिया गया है उस पर पूर्ण मन से विचार करो।
सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ।।६४ ।।
शब्दार्थ : सर्वगुह्यतमम् -सर्वाधिक रहस्यपूर्ण, भूयः-पुनः, शृणु सुनो, मे-मेरा, परमम् -परम, वचः- वचन, इष्टः-प्रिय, असि-हो, मे-मुझे, दृढम् - एकान्तिक, अत्यन्त, इति-इस प्रकार, ततः इसलिए, वक्ष्यामि कहूँगा, ते-तुम्हारे, हितम् - हित के लिए।
अनुवाद : तुम पुनः मेरे परम उपदेश को सुनो जो सर्वाधिक गोपनीय है। क्योंकि तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हो इसलिए तुम्हारे कल्याण की बात कहूँगा ।
व्याख्या : पुनः अनन्यमनस्क हो कर मुझे सुनो। तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हो। तुम सच्चे साधक हो। तभी तुम्हें यह सर्वाधिक गोपनीय रहस्य बताने जा रहा हूँ। रहस्यों के रहस्य को मुझसे श्रवण करो। तुम्हें अच्छी प्रकार समझाने के लिए पुनः कहूँगा, यद्यपि अनेक बार यह बात कह चुका हूँ। मुझे तुम से कोई उपहार नहीं लेना है। तुम मेरे सर्वाधिक प्रिय शिष्य और मित्र हो। इसलिए तुम्हारे हित की बात करूंगा। आत्म साक्षात्कार का साधन बताऊँगा। यही तुम्हारे लिए परम श्रेयस्कर और सर्वोच्च कल्याणकारी है।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।। ६५ ।।
शब्दार्थ : मन्मनाः मुझ में मन वाला, भव-हो, मद्भक्तः- मेरा भक्त, मद्याजी-मेरे लिए यज्ञ करो, माम् -मुझे, नमस्कुरु-प्रणाम करो, माम् -मुझे, एव-ही, एष्यसि-प्राप्त करोगे, सत्यम् -सत्य, ते-तुम्हें, प्रतिजाने-वचन देता हूँ, प्रियः-प्रिय, असि-हो, मे-मुझे।
अनुवाद : अपना मन मुझ में स्थिर करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे प्रणाम करो, इस प्रकार तुम मेरे ही निकट आओगे (मेरा सान्निध्य प्राप्त करोगे), मैं तुम्हें इस बात का सत्य वचन देता हूँ क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो ।
व्याख्या : मन की एकाग्रता का विकास करो। अपना मन मुझमें एकाग्र करो । मन इतस्ततः दौड़े तो पुनः अभ्यास द्वारा उसे ध्यान के केन्द्र पर ले आओ । समस्त कर्म मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारी वाणी मेरे नाम का जप करे । तुम्हारे हाथ मेरे लिए कार्य करें, तुम्हारे पैर मेरे लिए ही गति करें। तुम्हारे सब कर्म मेरे लिए हों। किसी प्राणी के लिए घृणा-द्वेष का भाव मत रखो। मुझे वन्दन करो तब तुम मुझे ही प्राप्त करोगे ।
भगवान् अर्जुन को सुनिश्चित वचन देते हैं, उसके लिए उदात्त घोषणा करते हैं।
हे अर्जुन, अपना लक्ष्य और केवल आश्रय मुझे मानने पर निश्चित रूप से तुम मेरा सान्निध्य प्राप्त करोगे।
भगवान् के वचनों में श्रद्धा रखो और धर्मसंस्कारयुक्त प्रतिज्ञा करो। भगवान् को ही अपना आश्रय मानो, तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे।
भगवान् की शरण ही भक्ति का रहस्य है। अगले श्लोक में भगवान् आत्म समर्पण का विषय सार रूप में उद्घाटित करते हैं। (निरूपण -IX.34; XII.8)
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।।६६ ।।
शब्दार्थ : सर्वधर्मान् -सब धर्मों को, परित्यज्य-त्याग कर, माम् -मेरी, एकम् - एक, शरणम्-शरण, व्रज-लो, अहम् - मैं, त्वा-तुम्हें, सर्वपापेभ्यः सब पापों से, मोक्षयिष्यामि-मुक्त करूँगा, मा-मत, शुचः-शोक करो।
अनुवाद : सब धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा। चिन्ता मत करो।
व्याख्या : अध्याय दो के श्लोक सात में अर्जुन द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर भगवान् ने इस श्लोक में दिया है। प्रश्न था- "मुझे निश्चयपूर्वक बतायें, मेरे लिए क्या हितकर है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे उपदेश दीजिए।"
सर्वधर्मान्-धर्मिक कृत्य और अधार्मिक कृत्य भी। समस्त कर्म, शुभ और अशुभ दोनों, क्योंकि यहाँ समस्त कर्मों से संन्यास का उपदेश दिया जा रहा है।
मामेकं शरणं व्रज-यह भाव अद्वैत विचारधारा को प्रतिपादित करता है। “जान लो कि मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, मैं ही सब में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान हूँ। यदि तुम इस निष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा । तुम्हारे अपने ही आत्म तत्त्व के रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर के तुम्हें अधर्म और धर्म के बन्धन से परे कर दूँगा।”
रूप का दर्शन चक्षु का धर्म है। सब रूपों का आधार ब्रह्म है। जब किसी विषय को देखो तो उसमें ब्रह्म दर्शन करो, विषय को त्याग दो, वह भ्रान्ति है और अनित्य है। अन्य इन्द्रियों के विषयों के प्रति भी इसी भाव को रखो। जीव धर्म त्याग दो जैसे-"मैं कर्मों का करने वाला (कर्ता) हूँ। मैं भोक्ता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ। मेरे पास अल्प ज्ञान और अल्प शक्ति है आदि" । स्वयं को ब्रह्म भावना में स्थिर करो अर्थात्- "मैं ब्रह्म हूँ" इस भाव को स्थिर करो। वेदान्त के अनुसार भगवान् कृष्ण में शरण लेना इसी को कहा है।
भगवान् के लिए अनवरत कर्म करो किन्तु कर्म फल भगवान् को समर्पित कर दो। उसे अपना एकाधार मानो । उसके लिए जियो। उसी का चिन्तन करो। उसका ही ध्यान करो। अपना जीवन, कर्म, भाव और विचार भगवान् में समाहित करो। तुम उसमें विश्राम पाओगे। तुम उससे एकत्व प्राप्त करोगे। तुम अमर, परम शान्ति और शाश्वत आनन्द प्राप्त करोगे। यह अन्य मतावलम्बियों की विचारधारा है।
शंकराचार्य इस तथ्य का दृढ़तापूर्वक निषेध करते हैं कि ज्ञान कर्म के साथ मिल कर मोक्ष का साधन हो सकता है। उनके विचार से कर्म और ज्ञान एक ही मनुष्य में साथ-साथ नहीं चल सकते क्योंकि कर्म हृदय को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है और आत्मा का यथार्थ ज्ञान ही उसे संसार से पूर्णतया मुक्त करने में समर्थ है। उनके अनुसार कर्म और ज्ञान, अन्धकार और प्रकाश के समान हैं और कर्म तो इस मिथ्या प्रपञ्च (दृश्य सत्ता) में ही सम्भव है जो अविद्या का विस्तार है तथा अविद्या रूपी अन्धकार का निराकरण ज्ञान रूपी प्रकाश से होता है। (निरुपण - III.30 .IX.22)
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ।।६७ ।।
शब्दार्थ : इदम् - यह, ते-तुम्हारे, न-नहीं, अतपस्काय-तप रहित, न-नहीं, अभक्ताय-अभक्त (के लिए), कदाचन-कभी भी, न-नहीं, च-और, अशुश्रूषवे-जो सुनने का इच्छुक न हो, वाच्यम् -कहना चाहिए, न-नहीं, च और, माम्-मुझे, यः जो, अभ्यसूयति-जो छिद्रान्वेषण करता है अथवा मुझमें दोषदृष्टि रखता है।
अनुवाद : यह सन्देश किसी ऐसे व्यक्ति को कभी मत कहना जिसने तप न किया हो, जिसमें भक्ति भाव न हो, जिसमें सेवा भाव न हो अथवा जो सुनने का इच्छुक न हो और जो मेरे प्रति दोष दृष्टि रखता हो (मुझे ईश्वर न जानने से मुझ में आत्मप्रशंसा आदि दोषों का अध्यारोपण करके मेरे ईश्वरत्व को सहन न करता हो)।
व्याख्या : इदम् - यह शास्त्र जिसका तुम्हें आदेश दिया गया है। शुश्रूषा-गुरु की।
यह शास्त्र प्रत्येक के लिए नहीं है। इसका उपदेश केवल उसी को दिया जाना चाहिए जो ईश्वर में दोष दृष्टि नहीं रखखता, जो तपस्वी है, भक्त है, जो श्रवण की पिपासा (जिज्ञासा) से युक्त है और जो गुरु निष्ठ है अर्थात् गुरु सेवा में तत्पर रहता है।
मां यः अभ्यसूयति-जो मुझे साधारण मानव समझ कर मेरा अनादर करता है और मेरे ईश्वरत्व में शंका करता है अर्थात् कोई मुझे ईश्वर कहे उसे अच्छा नहीं लगता।
य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ।।६८ ।।
शब्दार्थ : यः-जो, इमम्-यह, परमम् -परम, गुह्यम् गोपनीय, मद्भक्तेषु मेरे भक्तों में, अभिधास्यति-कहेगा (सुनायेगा), भक्तिम् - भक्ति, मयि- मुझ में, पराम् -परम, कृत्वा कर के, माम् -मुझ को, एव-ही, एष्यति-प्राप्त होगा, असंशयः - निस्सन्देह ।
अनुवाद : मेरे प्रति परम भक्ति भाव रख के जो मनुष्य मेरे भक्तों को यह परम गोपनीय ज्ञान सुनायेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा इसमें संशय नहीं है।
व्याख्या : इमं परमं गुह्यम् -कृष्णार्जुन संवाद रूप में उपर्युक्त गीता ज्ञान का गोपनीय उपदेश। इसे परम गुह्य क्यों कहते हैं? क्यों कि यह ज्ञान अमृतत्व प्राप्ति में और संसार चक्र से मुक्त होने में सहायक है।
भक्तिभाव से पूर्ण मनुष्य ही गीता का उपदेश श्रवण करने के लिए योग्य है। अभिधास्यति-कहेगा । भगवान् में परम गुरु का भाव रख कर और गुरु सेवा समझ कर जो इस ग्रन्थ को सुनायेगा (वह मुझे प्राप्त होगा) ।
असंशयः - इसका अर्थ यह भी हो सकता है-"संशयों से मुक्ति।"
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ।।६९ ।।
शब्दार्थ : न-नहीं, च-और, तस्मात्-उससे, मनुष्येषु-मनुष्यों में, कश्चित्-कोई, मे मेरा, प्रियकृत्तमः- मेरा अतिशय प्रिय करने वाला, भविता-होगा, न नहीं, च-और, मे-मेरा, तस्मात्-उससे, अन्यः- अन्य, प्रियतरः- अधिक प्रिय, भुवि-भूलोक में।
अनुवाद : मनुष्यों में उससे अधिक प्रियतर मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं और इस धरा पर उससे अधिक प्रिय भी मुझे और कोई नहीं होगा।
व्याख्या : यह गीता ग्रन्थ का ज्ञान मेरे भक्तों में वितरित करने वाला मेरी अत्यधिक सेवा करता है। वह मुझे अत्यन्त प्रिय है। वर्तमान पीढ़ी में मेरी इससे बढ़कर प्रियतर सेवा करने वाला न कोई है और न ही भविष्य में, इस विश्व में होगा।
भुवि-धरा पर, विश्व में।
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ।।७० ।।
शब्दार्थ: अध्येष्यते-अध्ययन करेगा, च-और, यः जो, इमम् -इस, धर्म्यम् -पावन, संवादम् -संवाद को, आवयोः- हम दोनों के, ज्ञानयज्ञेन-ज्ञान यज्ञ के द्वारा, तेन-उसके द्वारा, अहम् -मैं, इष्टः- पूजित, स्याम् - होऊँगा, इति-इस प्रकार, मे-मेरी, मतिः- मति (हैं)।
अनुवाद : और जो मनुष्य हम दोनों के इस पावन संवाद का अध्ययन करेगा, वह मानो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है।
व्याख्या : यज्ञ चार प्रकार के हैं-विधि यज्ञ, जप यज्ञ, उपांशु यज्ञ और मानस यज्ञ । विधि यज्ञ-अनुष्ठान क्रिया आदि है। मन्त्रोच्चारण जप यज्ञ है। निम्न स्वर से मन्त्रोच्चारण उपांशु यज्ञ है। चतुर्थ है मानस यज्ञ जो बिना ओष्ठ हिलाये मन से किया जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। गीता की स्तुति ज्ञान यज्ञ है।
श्रद्धा और भक्ति से इस ग्रन्थ का अध्ययन करने वाला ज्ञान यज्ञ करने का अथवा देवतादि का ध्यान करने का फल प्राप्त करेगा।
श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।
सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ।।७१ ।।
शब्दार्थ : श्रद्धावान् श्रद्धा युक्त, अनसूयः - ईर्ष्या रहित, च - और , शृणुयात् सुनेगा, अपि-भी, यः- जो, नरः- मनुष्य, सः वह, अपि-भी, मुक्तः मुक्त, शुभान् शुभ, लोकान् लोकों को, प्राप्नुयात् प्राप्त करेगा, पुण्यकर्मणाम् - पुण्यात्माओं के ।
अनुवाद : ईर्ष्या रहित और श्रद्धायुक्त हो कर जो भी मनुष्य इस ग्रन्थ का (गीता-ज्ञान का) श्रवण करेगा, वह भी मुक्त हो कर पुण्यात्माओं के लोक को प्राप्त करेगा।
व्याख्या : मुक्तः- पाप मुक्त ।
पुण्यकर्मणाम् - अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म करने वालों के।
सोऽपि वह भी। अधिक तो क्या, जो गीता के उपदेश का अवगाहन करता है, उसे समझता है, इसके भाव में रहता है और इसमें निहित अमूल्य उपदेशों का पालन करता है वह पुण्यकर्मी है।
कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ।।७२ ।।
शब्दार्थ : कच्चित् -क्या, एतत्-इस, श्रुतम् -सुना गया, पार्थ-हे पार्थ, त्वया-तुम्हारे द्वारा, एकाग्रेण - एकाग्रचित्त हो कर, चेतसा-चित्त से, कच्चित् -क्या, अज्ञानसंमोहः-अज्ञान रूपी मोह, प्रनष्टः- नष्ट हुआ, ते तुम्हारा, धनञ्जय-हे धनञ्जय ।
अनुवाद : हे पार्थ, क्या तुमने इस ज्ञान को एकाग्रचित्त होकर सुना? हे धनञ्जय, क्या तुम्हारा अविद्या जनित मोह नष्ट हुआ?
व्याख्या : गुरु का यह कर्तव्य है कि वह शिष्य को इस प्रकार से पाठन कराये कि शिष्य ग्रन्थ के निहितार्थ को भली प्रकार ग्रहण कर सके और जीवन के लक्ष्य (मोक्ष) को भी प्राप्त करने में सफल हो सके। यदि शिष्य समझ नहीं रहा तो गुरु अथवा आचार्य को उपमा, अनुरूप दृष्टान्त अथवा अन्य निर्देशों से उसका स्पष्टीकरण करना होगा। इसीलिए तो भगवान् कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं- "क्या तुम्हारा अविद्या रूपी मोह नष्ट हो गया है?"
एतत् - यह अर्थात् जो मैंने तुम्हें बताया है।
हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्रचित्त हो कर श्रवण किया है? क्या तुमने मेरे उपदेशों को ग्रहण कर लिया है?
अज्ञान संमोहः अविद्याजनित विवेकशून्यता जो स्वाभाविक है। क्या तुम्हारा मूढ़ भाव विनष्ट हो गया जिसके कारण तुमने शास्त्र श्रवण का परिश्रम किया और मेरा गुरु के सम्बन्ध से शास्त्रोपदेश विषयक परिश्रम हुआ है?
अर्जुन उवाच
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।। ७३ ।।
शब्दार्थ : नष्टः नष्ट हो गया, मोहः- मोह, स्मृतिः स्मृति (ज्ञान), लब्धा-प्राप्त कर के, त्वत्प्रसादात्-आपकी कृपा से, मया-मेरे द्वारा, अच्युत-हे कृष्ण, स्थितःअस्मि-स्थित हूँ, गतसन्देहः- शंका रहित हो कर, करिष्ये-पालन करूँगा, वचनम् वचन, तव-आपके ।
अर्जुन ने कहा
अनुवाद : हे कृष्ण, आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर के मेरा मोह नष्ट हो गया है और इस स्मृतिलाभ से मेरे समस्त संशय विच्छिन्न हो गये हैं। अब मैं आपके वचन (आज्ञा) का पालन करूँगा।
व्याख्या : मोहः- जीवों को वशीभूत करने के लिए माया का यह सर्वाधिक प्रभावशाली शस्त्र है। इसकी उत्पत्ति का मूल यही मोह है। मोहातीत होना सागर को पार करने के समान दुष्कर है।
स्मृतिः- मैंने आत्मा की यथार्थ प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आध्यात्मिक साधना और शास्त्राध्ययन का पूर्ण उद्देश्य मोह का विनाश और आत्म-ज्ञान की प्राप्ति है। ऐसी उपलब्धि होने पर अविद्या की तीन ग्रन्थियाँ-अज्ञान, मोह और कर्म, नष्ट होती हैं। समस्त संशय मिट जाते हैं। सारे कर्म अवसान को प्राप्त होते हैं, शेष कुछ करने को नहीं रह जाता।
ईशावास्योपनिषद् में इस विषय में कहा है-
"तन्त्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः" ई.उ.७.
"एकत्व की अनुभूति करने वाले को मोह कैसा और शोक कैसा?"
करिष्ये वचनं तव-अर्जुन कहना चाहता है- "मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए कृत संकल्प हूँ। आपकी कृपा से मैंने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब और कुछ करने को शेष नहीं रहा।"
सञ्जय उवाच
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ।।७४ ।।
शब्दार्थ : इति-इस प्रकार, अहम् -मैंने, वासुदेवस्य-कृष्ण का, पार्थस्य -पार्थ का (अर्जुन का), च-और, महात्मनः- महान् आत्मा का, संवादम् - संवाद, इमम् यह, अश्रौषम् -सुना, अद्भुतम्-अद्भुत, रोमहर्षणम् -रोमांचकारी ।
सञ्जय ने कहा
अनुवाद : इस प्रकार मैंने भगवान् कृष्ण और महात्मा अर्जुन का अद्भुत, अलौकिक, रोमांचकारी संवाद सुना ।
व्याख्या : अद्भुत योग और भावातीत आध्यात्मिक विषयों से सम्बद्ध गोपनीय शाश्वत ज्ञान होने के कारण यह अद्भुत है, विस्मयकारी है।
जब कभी उच्चतर कल्याणकारी शुभ भाव अन्तःकरण में अभिव्यक्त होते हैं, साधक पुलकित हो उठता है। भक्त प्रायः इस रोमहर्षण की अनुभूति करते हैं।
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ।।७५ ।।
शब्दार्थ : व्यासप्रसादात् - भगवान् व्यास के अनुग्रह से, श्रुतवान् - (मैंने) सुना, एतत् यह, गुह्यम् -रहस्यपूर्ण, अहम् -मैंने, परम् -परम, योगम्योग, योगेश्वरात् योगेश्वर से, कृष्णात् -कृष्ण से, साक्षात् साक्षात्, कथयतः-कहते हुए, स्वयम् स्वयम् ।
अनुवाद : भगवान् व्यास की कृपा से मैंने यह परम गोपनीय योग योगेश्वर कृष्ण से साक्षात् स्वयं कहते हुए सुना है।
व्याख्या : व्यास प्रसादात्-व्यास जी की कृपा से दिव्यचक्षु प्राप्त करके ।
योग-कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी योग को मैंने साक्षात् भगवान् कृष्ण से सुना है (परंपरा से नहीं) । योग विषयक होने के कारण यह संवाद ही योग है और यह भगवान् से एकत्व की प्राप्ति कराने वाला है।
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ।।७६ ।।
शब्दार्थ : राजन् -हे राजन्, संस्मृत्य-स्मरण कर के, संस्मृत्य-स्मरण कर के, संवादम् -संवाद को, इमम्-इस, अद्भुतम् - विस्मयकारी, केशवार्जुनयोः- केशव और अर्जुन का, पुण्यम् -पावन, हृष्यामि - हर्षित हो रहा हूँ, च-और, मुहुः पुनः, मुहुः पुनः ।
अनुवाद : हे राजन्, केशव और अर्जुन के इस अद्भुत, पावन संवाद को पुनः पुनः स्मरण कर के मैं पुलकित हो रहा हूँ।
व्याख्या : राजन् राजा धृतराष्ट्र जिनको संजय ने गीता सुनाई।
पुण्यम् - श्रवण मात्र से साधक के पाप पुंज को नष्ट करने वाला, श्रोता को पवित्र और ईश्वरोन्मुख करने वाला होने के कारण यह पावन है।
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।
विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ।।७७ ।।
शब्दार्थ : तत्वह, चऔर, संस्मृत्य-स्मरण कर के, संस्मृत्य-स्मरण कर के, रूपम् -रूप, अत्यद्भुतम् - अति अद्भुत, हरेः- हरि का, विस्मयः- आश्चर्य, मे—मेरा, महान् -महान्, राजन्- हे राजन्, हृष्यामि - हर्षित हो रहा हूँ, च-और, पुनः पुनः पुनः पुनः ।
अनुवाद : और हे राजन्, हरि के उस अत्यन्त अद्भुत स्वरूप को भी बारम्बार स्मरण कर के मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ।
रूपम् - विश्वरूप (अध्याय XI)
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।।७८ ।।
शब्दार्थ : यत्र-जहाँ, योगेश्वरः- योगेश्वर, कृष्णः-कृष्ण, यत्र-जहाँ, पार्थः अर्जुन, धनुर्धरः- धनुर्धारी, तत्र वहाँ, श्रीः समृद्धि, विजयः-विजय, भूतिः - विभूति, प्रसन्नता, ध्रुवा-अचल, नीतिः-नीति, मतिः-मति, मम-मेरी।
अनुवाद : जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहीं श्री, विजय, विभूति और दृढ़ नीति का साम्राज्य है, यह मेरा मत है।
व्याख्या : यह श्लोक 'एकश्लोकी गीता' नाम से अभिहित है अर्थात् सम्पूर्ण भगवद्गीता एक श्लोक में। केवल इसी श्लोक की पुनरावृत्ति सम्पूर्ण शास्त्र के पढ़ने का लाभ प्रदान करती है।
यत्र-जिस पक्ष में।
योगेश्वरः-योग के ईश्वर । भगवान् कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है क्योंकि सब प्रकार के योग के बीजों का उद्भव उन्हीं से है।
धनुर्धरः गाण्डीव धारण करने वाले (अर्जुन) । तत्र-पाण्डवों के पक्ष में।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ।।
।। इति मोक्षसंन्यासयोगः ।।
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !
परिशिष्ट
१.गीता में भगवान् के आदेश
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ।।२/३।।
१. (इस समय) हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त होना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। हे शत्रु को सन्तप्त करने वाले (अर्जुन), हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ।
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ।।२/१४।।
२. हे कुन्तीपुत्र, इन्द्रिय-विषयों के संयोग तो उत्पत्ति- विनाशशील तथा अनित्य हैं और सरदी-गरमी एवं सुख-दुःख के देने वाले हैं। इन्हें सहन करो।
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ।।२/१८।।
३. नित्य, अविनाशी, अप्रमेय शरीरधारी जीवात्मा के ये शरीर नश्वर हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।।२/३७ ।।
४. मारे जाने पर स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे और विजय प्राप्त करने पर धरती का राज्य भोगोगे । अतः हे कुन्तीपुत्र, उठो, युद्ध के लिए संकल्प करो।
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।।२/३८ ।।
५. सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय में समभाव रह कर अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।२/४७ ।।
६. तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की इच्छा करने का कदापि नहीं। तुम्हारा उद्देश्य कर्म-फल की प्राप्ति न हो और न ही कर्म के त्याग (अकर्म) में तुम्हारा अनुराग हो ।
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।।२/४८।।
७. हे अर्जुन, जय-पराजय की आसक्ति त्याग कर योग में स्थित हो कर कर्म करो। मन का समत्व ही योग कहलाता है।
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ।।२/५० ।।
८. बुद्धिमान् मनुष्य इसी जन्म में अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, योग-मार्ग का अनुसरण करो। योग में संलग्न हो जाओ। कर्म में कुशलता ही योग है।
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।।३/१९ ।।
९. इसलिए आसक्ति रहित हो कर तुम कर्तव्य कर्म को करो; क्योंकि आसक्ति का त्याग कर के कर्म करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है।
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।।३/३०।।
१०. समस्त कर्म मुझे समर्पित कर के, चेतना को आत्मा में स्थिर कर के, आशा (इच्छा) और अहंकारशून्य हो कर, निरुद्वेग हो कर तुम युद्ध करो।
परिशिष्ट
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ।।३/४१ ।।
११. अतः, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ (अर्जुन), पहले इन्द्रियों को वश में करो। तत्पश्चात् ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को मार डालो।
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ।।३/४३ ।।
१२. एवंविध, हे अर्जुन, उसे जान कर, जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है और आत्मा से आत्मा को संयत कर के, हे महाबाहु, तुम दुर्जेय काम रूपी शत्रु को जीत लो।
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनाऽऽत्मनः ।
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।।४/४२ ।।
१३. इसलिए हे अर्जुन, उठो, योग की शरण लो और अज्ञानवश हृदय में उत्पन्न सन्देह को आत्म-ज्ञान की तलवार से छिन्न-भिन्न कर दो।
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ।।६/२६ ।।
१४. जिस-जिस निमित्त से यह चञ्चल और अस्थिर मन इतस्ततः भटकता है, उसी से हटा कर, वश में कर के (साधक) आत्मा में स्थित करे ।
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगीस्माद्योगी भवार्जुन ।।६/४६ ।।
१५. योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी ही श्रेष्ठ है; अतः हे अर्जुन, योगी बनो।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ।।८/७ ।।
१६. इसलिए समस्त कालों में मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो। मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर के तुम निस्सन्देह मुझे ही प्राप्त करोगे ।
नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।।८/२७ ।।
१७. हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों का ज्ञान होने पर योगी मोहित नहीं होता, इसलिए, हे पार्थ, तुम सब कालों में योग युक्त रहो अर्थात् योगी बनो ।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ।।८/(२७) ।।
१८. जो भी भक्त भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है, पवित्र मन से और भक्ति भाव से अर्पण की उस भेंट को मैं स्वीकार करता हूँ।
किं पुनर्बाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ।।९/३३।।
१९. और कितना (सहज रूप से) ब्राह्मण और राजर्षि भक्त लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस दुःखद क्षणभङ्गुर लोक को प्राप्त कर के अब तुम मेरी आराधना करो।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ।।९/३४।।
२०. अपना मन मुझ में एकाग्र करो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यजन करो, मुझे प्रणाम करो । इस प्रकार पूर्ण मन से मेरे परायण हो कर मुझे ही अपना लक्ष्य मान कर तुम मुझे प्राप्त करोगे।
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ।। ११/८।।
२१. किन्तु अपने इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। मेरी ईश्वरीय योग-शक्ति के दर्शन करो।
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व
जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् ।
मयैवैते निहताः पूर्वमेव
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ।।११/३३ ।।
२२. इसलिए, उठो और यश प्राप्त करो। शत्रु को जीत कर अप्रतिम राज्य का उपभोग करो। हे अर्जुन, निश्चित रूप से वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त बनो।
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णं तथाऽन्यानपि योधवीरान् ।
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ।।११/३४ ।।
२३. द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और अन्य शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अब तुम भय से विचलित न हो कर इन्हें मारो। युद्ध करो, तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे।
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ।। १२/८।।
२४. अपना मन मुझ में ही एकाग्र करो, अपनी बुद्धि भी मुझ में ही स्थिर करो। इसके पश्चात् तुम मुझ में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं।
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।।१६/२४।।
२५. अतः कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण हैं। वेद-शास्त्रों में विहित अध्यादेश का ज्ञान कर के तुम्हें इस संसार में कर्म करना चाहिए।
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ।।१८/५७ ।।
२६. विवेक-बुद्धि से सब कर्म मुझे समर्पित कर के, मुझे ही सर्वोच्च लक्ष्य मान कर, बुद्धियोग का आश्रय ले कर तुम अपना मन सदा मुझ में स्थिर करो।
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ।।१८/६२ ।।
२७. हे अर्जुन, तुम पूर्ण भाव से (अपने सम्पूर्ण अस्तित्व से) उसी की शरण में जाओ। उस प्रभु की अहेतुकी कृपा से तुम परम शान्ति और शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।।१८/६५।।
२८. अपना मन मुझ में स्थिर करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे प्रणाम करो, इस प्रकार तुम मेरे ही निकट आओगे (मेरा सान्निध्य प्राप्त करोगे), मैं तुम्हें इस बात का सत्य वचन देता हूँ; क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो।
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।।१८/६६ ।।
२९. सब धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा। चिन्ता मत करो।
२.उद्बोधक उपदेश
भगवान् कृष्ण ने निम्नांकित श्लोकों में इन उपमा अलंकारों का प्रयोग किया है :
१. जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जीर्ण-शीर्ण वस्त्रों को उतार कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह देहधारी आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है। ( २/२२ )
२. सब ओर जल ही जल होने पर एक जलाशय का जितना महत्त्व रह जाता है, उतना ही महत्त्व अथवा प्रयोजन एक ज्ञानी ब्राह्मण का वेदों से होता है। (२/४६)
३. चारों ओर से अपने अङ्गों का संहरण कर लेने वाले कछुए की भाँति जब कोई पुरुष इन्द्रियों के विषयों से अपनी इन्द्रियों को विमुख कर लेता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला, प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला कहलाता है। (२/५८)
४. जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण अचल, स्थिर सागर में जल (उसे क्षुब्ध किये बिना) प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य में सब कामनाएँ उसे विचलित किये बिना प्रवेश कर जाती हैं, वह शान्ति को प्राप्त करता है, कामनाओं का इच्छुक नहीं। (२/७०)
५. हे भारत (अर्जुन), जिस प्रकार से एक अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त हो कर कर्म करता है, उसी प्रकार से एक विद्वान् पुरुष लोक-कल्याणार्थ आसक्ति रहित हो कर कर्म करे। (३/२५)
६. जिस प्रकार अग्नि धुएँ से, दर्पण धूल से और गर्भ ज़ेर से ढके रहते हैं, उसी प्रकार यह (ज्ञान) उससे (रजोगुण से) ढका रहता है ।(३/३८)
७. इस दिव्य ज्ञान को पा कर ही पुरातन काल में मुमुक्षु जनों ने कर्म किये; इसलिए तुम भी अपने पूर्वकाल के पूर्वजों की भाँति अनासक्त भाव से कर्म करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। (४/१५)
८. हे अर्जुन, जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। (४/३७)
९. अनासक्त हो कर परमात्मा को समर्पित करके कर्म करने वाला मनुष्य जल में कमल-पत्र की भाँति पाप से लिप्त नहीं होता। (५/१०)
१०. आत्मा के साथ संयोग करने का अभ्यास करने वाले जितेन्द्रिय योगी की उपमा उस दीपक से की जाती है जो वायु रहित स्थान में स्थित होने के कारण लोलित (चलायमान) नहीं होता। (६/१९)
११. निश्चित रूप से मन चञ्चल, उच्छृंखल, बलवान् और हठीला है। हे कृष्ण, इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान कठिन है। (६/३४)
१२. हे महाबाहो (कृष्ण), दोनों ओर से पतित, आश्रय रहित हो कर ब्रह्म के मार्ग में भ्रमित (किंकर्तव्यविमूढ़) हो कर छिन्न-भिन्न बादल की भाँति नष्ट तो नहीं हो जाता? (६ /३८)
१३. इन दोनों प्रकृतियों को समस्त प्राणियों की योनियाँ ही समझो। अतः मैं ही इस जगत् का उद्भव और प्रलय हूँ। (७/७)
१४. जिस प्रकार सर्वत्र विचरण करने वाला वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार सारे प्राणी मुझमें स्थित हैं, ऐसा जानो। (९/६)
१५. आकाश में यदि एक सहस्र सूर्यों का तेज एक साथ प्रकाशित तो वह तेज भी कदाचित् ही उस महान् विश्वरूप पुरुष का हो। (११/१२)
१६. जिस प्रकार नदियों की वेगपूर्ण धारायें समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार नरलोक के ये वीर प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। (११/२८)
१७. जिस प्रकार (मोहवश) पतने अपने ही विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में अत्यन्त वेग से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये प्राणी अपने विनाश हेतु अत्यन्त वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। (११/२९)
१८. हे कुन्तीपुत्र (अर्जुन), यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है उसे तत्त्वज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। (१३/१)
१९. सर्वव्यापक आकाश जिस प्रकार से सूक्ष्मता के गुण के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा शरीर में सर्वत्र होते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता। (१३/३२)
२०. हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य समस्त ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार परमात्मा, क्षेत्र का स्वामी, सम्पूर्ण क्षेत्र (शरीर) को प्रकाशित करता है। (१३/३३)
२१. वे (विद्वज्जन) अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष को ऊपर मूल और नीचे शाखा वाला कहते हैं, जिसके पत्ते छन्द अर्थात् ऋचायें हैं। जो इसे जानता है, वह वेदों को जानने वाला है (वेदज्ञ है)। (१५/१)
२२. गुणों द्वारा पोषित इसकी शाखायें नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। इन्द्रियों के विषय कलिका (कलियाँ) हैं। नीचे मनुष्य-लोक पर्यन्त इसकी जड़ें (मूल) विस्तृत हैं जो कर्म-बन्धन में डालने वाली हैं। (१५/२)
२३. जीवात्मा जो शरीर धारण करता है, उसका उत्क्रमण करते समय वह इन (इन्द्रियों और मन) को उसी प्रकार अपने साथ ले जाता है, जिस प्रकार वायु अपने आश्रय-स्थल (फूलों आदि) से गन्ध को साथ ले जाता है। (१५ / ८)
२४. मुझमें अपना चित्त स्थिर करके, मेरी कृपा से तुम सब बाधाओं को पार कर जाओगे और यदि अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे, तो नष्ट हो जाओगे । (१८ / ५८)
परिशिष्ट
२५. हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और शरीर रूपी यन्त्र पर आरूढ़ इन प्राणियों को अपनी माया की शक्ति से उनके कर्मानुसार भ्रमाता है। (१८/६१)
विशेष : ११, १२, १६ और १७ भगवान् कृष्ण को कहे गये अर्जुन के वचन हैं।
३.सप्तश्लोकी गीता
१. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ।।८/१३।।
२. स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ।।११/३६ ।।
३. सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।।१३/१३ ।।
४. कविं पुराणमनुशासितार- मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।।८/९ ।।
५. ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ।।१५/१।।
६. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ।।१५/१५ ।।
७. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ।।९/३४ ।।
४. एकश्लोकी गीता
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।।
५. प्रतिज्ञा गीता
(भगवान् का आश्वासन)
भगवद्गीता मानवता के लिए सुख, शान्ति, मोक्ष, पूर्णत्व और ऐश्वर्य का सन्देश देती है। केवल गीता ही ऐसा ग्रन्थ है जो साधक को प्रत्येक अवस्था में सहायता और हर प्रकार के भय से रक्षा प्रदान करने वाला है। गीता में भगवान् निम्नांकित आश्वासन देते हैं :
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।
इस योग में कोई भी प्रयास विफल नहीं होता और न ही कोई बाधा आती है (अर्थात् विपरीत परिणामों की उत्पत्ति अथवा उल्लंघन नहीं होते)। इस ज्ञान का थोड़ा-सा पालन भी महान् भय से रक्षा करता है। (२/४०)
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गतिं तात गच्छति ।।
हे अर्जुन, न तो इस लोक में न ही परलोक में उसका विनाश सम्भव है। प्रिय पुत्र, अच्छे कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्दशा को प्राप्त नहीं होता । (६/४०)
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।।
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो कर शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। (९/३१)
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।।
अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करने वाले और मेरी ही आराधना करने बाले नित्ययुक्त साधकों का योग-क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। (९/२२)
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ।।
यदि तुम अन्य पापियों से भी अपेक्षाकृत अधिक पापी हो, तो भी निश्चित रूप से ज्ञान रूपी नौका द्वारा पाप के सागर से तर जाओगे। (४/ ३६)
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।।
अपना मन मुझमें स्थिर करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे प्रणाम करो, इस प्रकार तुम मेरे ही निकट आओगे (मेरा सान्निध्य प्राप्त करोगे), मैं तुम्हें इस बात का सत्य वचन देता हूँ ; क्योंकि तुम . मुझे प्रिय हो । (१८/६५)
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ।।
हे अर्जुन, उन मुझमें चित्त लगाने वाले भक्तों के लिए मैं अचिरेण ही इस मर्त्यलोक रूप सागर से समुद्धार करने वाला होता हूँ। (१२/७)
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।।
सब धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा। चिन्ता मत करो। (१८/६६)
६. गीता-अनुष्ठान
गीतानुष्ठान करने वाले साधकों को अनुष्ठान की अवधि में इन नियमों का पालन करना चाहिए-
१. प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त में चार बजे उठना ।
२. हल्का सात्त्विक आहार दिन में केवल एक बार मध्याह्न में।
३. ब्रह्मचर्य का पालन ।
४. मौन अथवा मितभाषण का व्रत और सत्यभाषण ।
५. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का अनवरत मानसिक जप ।
दैनिक शौच के उपरान्त स्नान करो। शुद्ध वस्त्र धारण करो। स्वच्छ, पवित्र स्थान पर कुशासन बिछाओ। पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठो। नित्य कर्म-सन्ध्या-वन्दन, जप, ध्यान आदि पहले पूर्ण करो। भगवान् कृष्ण के १०८ अथवा १२ नामों की पुनरावृत्ति करो अर्थात् १०८ बार अथवा १२ बार भगवान् कृष्ण के नाम का जप करो। तत्पश्चात् श्री कृष्ण का ध्यान करो । अब संकल्प करो (जिस प्रयोजन से अनुष्ठान कर रहे हैं) । करन्यास और अङ्गन्यास करो (इनकी विधि प्रारम्भिक पृष्ठों में दी गयी है) । करन्यास और अङ्गन्यास उसी मन्त्र से करना है जिसका तुम जप करने लगे हो। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' से भी न्यास हो सकते हैं।
इसके उपरान्त भगवान् श्री कृष्ण, व्यास और गीता की पूजा करो और षोडशोपचार करो। जप अविचलित, एकाग्र मन से पूर्ण श्रद्धा-भक्ति के साथ करना चाहिए। जप करते समय बीच में बोलना, कोई ध्वनि करना अथवा संकेत करना वर्जित है। जप करते समय इधर-उधर देखना, मुड़ना और हिलना नहीं चाहिए तथा एक ही आसन में स्थिर हो कर बैठना चाहिए। मन में एकमात्र भगवान् का ही विचार होना चाहिए। एक अनुष्ठान में यदि आकाङ्क्षित प्रभाव न मिले, तो निष्ठा समाप्त नहीं होनी चाहिए। श्रेयस्कर तो यह है कि भगवत्कृपा-प्रसाद की प्राप्ति के लिए तीन बार अथवा सात बार अनुष्ठान की पुनरावृत्ति हो ।
जप के अन्त में मन्त्र जप के दशम भाग की आहुति दे कर होम करना चाहिए। इसके पश्चात् उदकादि दान से (देवतार्थ) आहुतियों का दशम भाग तर्पण करना चाहिए। अन्त में तर्पण के दशम भाग की गणना से अथवा यथासम्भव अधिकाधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। होम में आहुति घृत एवं seasamum, आटा, जव, चीनी और घी के मिश्रण से डालनी चाहिए। अतीव श्रद्धा और विनम्र भाव से भगवान् को गेहूँ की मधुर माँड (कांजी) अर्पित करनी चाहिए और अर्पण करते समय इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए- "एष बलिः श्री कृष्णाय नमः ।" अगले दिन वही माँड गाय को दे दें।
दैनिक जप और पूजा करने के पश्चात् भगवान् से अनुष्ठान की अवधि में हुई किसी प्रकार की भूल के लिए निम्न मन्त्रों से क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिए :
आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनम् ।
विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ।।
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ।
तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर ।।
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन ।
यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते ।।
अब साष्टाङ्ग प्रणाम करते समय इस मन्त्र को बोलें:
"अनया यथोपचारपूजया भगवान् श्रीकृष्णः प्रियताम।"
इसके पश्चात् निम्न मन्त्र का उच्चारण करते हुए चरणामृत ग्रहण करें और सिर पर धारण करें:
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम् ।
सर्वदुःखोपशमनं विष्णुपादोदकं शुभम् ।।
इससे अनुष्ठान का पूर्ण लाभ मिलेगा। कम-से-कम ४१ दिवस पर्यन्त अनुष्ठान, प्रतिदिन १०×१०८ बार (१० माला) मन्त्र जप करना
जप हेतु मंत्र
|
मन्त्र |
प्रभाव |
|
कार्पण्यदोषोपहत... |
आत्म-समर्पण भाव लाने के लिए |
|
एवं बुद्धेः परं... |
काम-क्रोध आदि शत्रुओं का नाश |
|
बहूनि मे व्यतीतानि... |
भक्ति में स्थिरता |
|
भोक्तारं यज्ञतपसां... |
साधना में बाधाओं का विनाश |
|
शनैः शनैरुपरमेत्... |
मनोजय |
|
यतो यतो निश्चरति... |
ध्यानार्थ युक्तता |
|
यो मां पश्यति सर्वत्र... |
भक्ति की पराकाष्ठा |
|
सर्वभूतस्थितं यो मां... |
विवेक की विवृद्धि |
|
मत्तः परतरं नान्यत्... |
सर्वत्र भगवद्दर्शन की योग्यता |
|
अभ्यासयोगयुक्तेन... |
कामादि शत्रु-नाश |
|
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां... |
योग-क्षेम की अवाप्ति |
|
पत्रं पुष्पं फलं... |
भगवद्दर्शन की योग्यता |
|
यत्करोषि यदश्नासि... |
दैवी कृपा की प्राप्ति |
|
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य... |
आत्म-समर्पण की योग्यता |
|
मन्मना भव मद्भक्तो... |
आत्म-समर्पण की योग्यता |
|
तेषां सततयुक्तानां... |
योगयुक्त होना |
|
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं... |
विवेक-प्राप्ति |
|
त्वमादिदेवः पुरुषः... |
भक्ति का विकास |
|
वायुर्यमोऽग्निः... |
मन का संयम |
|
नमः पुरस्तात्... |
मोह का विनाश |
|
पितासि लोकस्य... |
भगवान् को प्रसन्न करने की योग्यता |
|
तेषामहं समुद्धर्ता... |
भगवत्साक्षात्कार की योग्यता |
|
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि... |
भगवद्भक्ति |
|
सर्वतः पाणिपादं... |
अन्तःकरण की शुद्धि |
|
अहं वैश्वानरो भूत्वा... |
विवेक से ज्ञानोद्भव |
|
सर्वस्य चाहं हृदि... |
क्रोध की निवृत्ति |
|
यो मामेवमसंमूढो... |
भक्ति |
|
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि... |
बाधा-शमन |
|
सर्वधर्मान् परित्यज्य... |
आत्म-समर्पण |
|
यन्त्र योगेश्वरः.. |
भगवत्कृपा |
विशेष : पूर्ण मन्त्र गीता में से देखे जा सकते हैं। दिये गये शब्दों से मन्त्र प्रारम्भ होता है।
जप करते समय ध्यान भगवान् श्री कृष्ण पर होना चाहिए। विविध श्लोकों का जिस प्रकार से अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार पूर्ण गीता का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। सम्पूर्ण गीता के अनुष्ठान में विविध श्लोक विविध प्रयोजनों के लिए सम्पुट श्लोक के रूप में लिये जा सकते हैं। सम्पुट दो प्रकार के हैं। प्रथम तो यह कि गीता-पाठ में प्रत्येक श्लोक के पश्चात् सम्पुट श्लोक की पुनरावृत्ति की जाये और फिर गीता का श्लोक पढ़ा जाये। इसे सम्पुट जप अथवा सम्पुट पाठ कहते हैं। द्वितीय विधि यह है कि गीता के प्रत्येक श्लोक के पूर्व और पश्चात् सम्पुट श्लोक पढ़ें अर्थात् गीता का एक श्लोक पढ़ने के उपरान्त सम्पुट श्लोक दो बार पढ़ें, तब अगला श्लोक लें। इसे सम्पुटावली कहते हैं। यह सम्पुट से अधिक प्रभावशाली है।
व्यावहारिक रूप में गीता का प्रत्येक श्लोक ही मन्त्र है, जिसे सम्पुट श्लोक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा सुना जाता है कि एक सन्त ने गीता का प्रत्येक श्लोक सम्पुट श्लोक के रूप में प्रयोग करके गीता-अनुष्ठान के ७०० पुरुश्चरण पूर्ण किये और भगवत्-कृपा-प्रसाद से अनुगृहीत हुए। पुनरपि सम्पुट श्लोक के प्रयोग के लिए कुछ श्लोक नीचे दिये जाते हैं।
सम्पुट श्लोकों की सूची
|
श्लोक |
सम्पुट में प्रयोग का प्रभाव |
|
कार्पण्यदोषोपहत... |
आत्म-समर्पण की योग्यता |
|
मत्तः परतरं नान्यत्... |
सर्वत्र भगवान् का साक्षात्कार |
|
पत्रं पुष्पं फलं... |
भगवद्दर्शन की योग्यता |
|
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्रण |
भगवद्भक्ति |
|
अहं वैश्वानरो भूत्वा... |
विवेक से ज्ञान का उद्भव |
|
सर्वधर्मान् परित्यज्य... |
आत्म-समर्पण |
|
यत्र योगेश्वरः... |
कामनापूर्ति |
इनके अतिरिक्त अनेक अन्य श्लोक भी सम्पुट में प्रयोग किये जा सकते हैं। प्रत्येक गीता पाठ के प्रारम्भ से पूर्व और पश्चात् बारह माला अथवा कम-से-कम एक माला द्वादशाक्षर मन्त्र का जप, करन्यास और अङ्गन्यास उसी मन्त्र से करना चाहिए। इस जप के लिए ध्यान इनसे करें :
विष्णुं शारदचन्द्रकोटिसदृशं शंखं रथाङ्गं गदा-
मंभोजं दधतं सिताब्जनिलयं कान्त्या जगन्मोहनम् ।
आबद्धाङ्गदहारकुण्डलमहामौलिं स्फुरत्कंकणं
श्रीवत्सांकमुदारकौस्तुभधरं वन्दे मुनीन्द्रैः स्तुतम् ।।
इसके उपरान्त गीता के ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, संकल्प, विनियोग, करन्यास, अङ्गन्यास और ध्यान की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। प्रतिदिन सम्पूर्ण गीता का अध्ययन कर सकें, तो और अच्छा है। अथवा दो दिन में करें-नौ अध्याय प्रतिदिन । यह भी सम्भव न हो, तो ६ अध्याय प्रतिदिन करें। इस प्रकार ३ दिन में गीता पूर्ण करें। ७ दिवस में समाप्त करने के लिए यह क्रम अपनायें- (१) अध्याय १,२; (२) अध्याय ३-५; (३) अध्याय ६-८; (४) अध्याय ९,१०; (५) अध्याय ११-१३; (६) अध्याय १४-१६; (७) अध्याय १७,१८ । अन्यथा २ अध्याय प्रतिदिन पढ़ कर ९ दिन में समाप्त कर सकते हैं। यह भी सम्भव न हो, तो प्रतिदिन १ अध्याय पढ़ें।
यदि सम्पूर्ण गीता का अनवरत रूप से निरन्तर एक वर्ष पर्यन्त पाठ किया जाये, तो पाठ करने वाले को परम आनन्द की प्राप्ति होगी। सम्पूर्ण पाठ न्यास आदि सहित होना चाहिए।
यदि चालीस दिन तक संहार-क्रम में गीता पाठ तीन बार प्रतिदिन किया जाये, अर्थात् अध्याय १८ से प्रारम्भ कर के विपरीत क्रम में पढ़ते हुए अध्याय १ तक प्रतिदिन तीन बार किया जाये, तो बन्धन से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
स्थिति-क्रम में यदि गीता पाठ ४० दिवस पर्यन्त किया जाये अर्थात् अध्याय ६ से १८ और पुनः ५ से १ (विपरीत), तो प्रचुर धन-धाम होता है।
संहार-क्रम संन्यासियों के लिए है और स्थिति-क्रम गृहस्थ जनों के लिए निर्दिष्ट है।
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान करना चाहिए। उत्सुकतावश, परीक्षण के लिए अथवा दोष ढूँढ़ने के भाव से नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की आन्तरिक अशुद्धि अथवा पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से आयी बाधा के कारण सात अनुष्ठान पूर्ण करने पर भी यदि अभीप्सित फल की प्राप्ति न हो, तो निष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। आन्तरिक बाधायें यदि अत्यधिक हैं, तो प्रभाव शीघ्र नहीं मिलेगा। अनुष्ठान का प्रभाव भौतिक दृष्टि से अभिव्यक्त न भी हो, तो भी इसमें किंचित् भी सन्देह नहीं कि अन्तःकरण की शुद्धि होती ही है। निष्काम भाव से यदि अनुष्ठान किया जाये, तो आत्म-परिष्कृति और दैव-कृपा के अवतरण में संशय नहीं। कोई ऐसा कर्म नहीं, जिसका फल प्राप्त न हो। फिर गीता के अनुष्ठान की तो बात ही क्या, जो पूर्ण निष्ठा और एकाग्र मन से किया गया हो? प्रभाव निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान् कृष्ण के उपदेशानुसार श्रेयस्कर तो यही होगा कि अनुष्ठान निष्काम भाव से, केवल आत्म-साक्षात्कार हेतु किया जाये। अतः गीता का अध्ययन, पठन, जप और मनन सदा शुद्ध निष्काम भाव से करना हितकर है।
गीता पाठ के अन्त में, वराहपुराण में दिये गये गीता-माहात्म्य का पाठ करना चाहिए। यदि वह न कर सकें, तो महाभारत में गीता के तत्काल पश्चात् दिये गये माहात्म्य का पाठ अवश्य करें।
अनुक्रमणिकाएँ
१.श्लोकानुक्रमणिका
(अ)
श्लोक अध्याय श्लोक संख्या
अकीर्तिं चापि भूतानि…………. २ ३४
अक्षरं ब्रह्म परमं ८ ३
अक्षराणामकारोऽस्मि ………… १० १३
अग्निज्योतिरहः शुक्लः…………. ८ २४
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम्…………….. २ २४
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा ………………… ४ ६
अज्ञश्चाश्रद्धानश्च. ………….. ४ ४०
अत्र शूरा महेष्वासाः ………….. १ ४
अथ केन प्रयुक्तोऽयम्………… ३ ३६
अथ चित्तं समाधातुम्……………. १२ ९
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम्…………… २ ३३
अथ चैनं नित्यजातम्………… २ २६
अथवा बहुनैतेन………….. १० ४२
अथवा योगिनामेव…………… ६ ४२
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा……………… १ २०
अथैतदप्यशक्तोऽसि…………. १२ ११
अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा…………….. ११ ४५
अदेशकाले यद्दानम्……….. १७ २२
अद्वेष्टश सर्वभूतानाम् ………….. १२ १३
अधर्मं धर्ममिति या ………….. १८ ३२
अधर्माभिभवात् कृष्ण……….. १ ४१
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः …….. १५ २
अधिभूतं क्षरो भावः………. ८ ४
अधियज्ञः कथं कोऽत्र ………… ८ २
अधिष्ठानं तथा कर्ता. ……….. १८ १४
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् ……. १३ ११
अध्येष्यते च य इमम् . …….. १८ ७०
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो १ १६
अनन्तश्चास्मि नागानाम् १० २९
अनन्यचेताः सततम्. ८ १४
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ९ २२
अनपेक्षः शुचिर्दक्षः १२ १६
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्. १३ ३१
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् ११ १९
अनाश्रितः कर्मफलम् ६ १
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च १८ १२
अनुद्वेगकरं वाक्यम् १७ १५
अनुबन्धं क्षयं हिंसाम्. १८ २५
अनेकचित्तविभ्रान्ताः १६ १६
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् ११ १६
अनेकवक्त्रनयनम् . ११ १०
अन्तकाले च मामेव. ८ ५
अन्तवत्तु फलं तेषाम् ७ २३
अन्तवन्त इमे देहाः २ १८
अन्नाद्भवन्ति भूतानि. ३ १४
अन्ये च बहवः शूराः १ ९
अन्ये त्वेवमजानन्तः १३ २५
अपरं भवतो जन्म ४ ४
अपरे नियताहाराः ४ ३०
अपर्याप्तं तदस्माकम्. १ १०
अपरेयमितस्त्वन्याम्. ७ ५
अपाने जुह्वति प्राणम् ४ २९
अपि चेत्सुदुराचारः ९ ३०
अपि चेदसि पापेभ्यः ४ ३६
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च १४ १३
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः १७ ११
अभयं सत्त्वसंशुद्धिः १६ १
अभिसन्धाय तु फलम् १७ १२
अभ्यासयोगयुक्तेन ८ ८
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि १२ १०
अमानित्वमदम्भित्वम्. १३ ७
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः ११ २६
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति . ११ २१
अयतिः श्रद्धयोपेतः ६ ३७
अयनेषु च सर्वेषु. १ ११
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः १८ २८
अवजानन्ति मां मूढाः ९ ११
अवाच्यवादांश्च बहून् २ ३६
अविनाशि तु तद्विद्धि २ १७
अविभक्तं च भूतेषु. १३ १६
अव्यक्तादीनि भूतानि २ २८
अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः. ८ १८
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः . ८ २१
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् २ २५
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् ७ २४
अशास्त्रविहितं घोरम् . १७ ५
अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् २ ११
अश्रद्धानाः पुरुषाः . ९ ३
अश्रद्धया हुतं दत्तम् १७ २८
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् १० २६
असक्तबुद्धिः सर्वत्र. १८ ४९
असक्तिरनभिष्वङ्गः. १३ ९
असत्यमप्रतिष्ठं ते. १६ ८
असौ मया हतः शत्रुः १६ १४
असंयतात्मना योगः . ६ ३६
असंशयं महाबाहो ६ ३५
अस्माकं तु विशिष्टश ये . १ ७
अहमात्मा गुडाकेश १० २०
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः १६ १८
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्. १८ ५३
अहं क्रतुरहं यज्ञः ९ १६
अहं वैश्वानरो भूत्वा १५ १४
अहं सर्वस्य प्रभवः १० ८
अहं हि सर्वयज्ञानाम् ९ २४
अहिंसा सत्यमक्रोधः १६ २
अहिंसा समता तुष्टिः १० ५
अहो बत महत्पापम्. १ ४५
(आ)
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः ११ ३१
आचार्याः पितरः पुत्राः १ ३४
आढ्योऽभिजनवानस्मि १६ १५
आत्मसंभाविताः स्तब्धाः. १६ १७
आत्मौपम्येन सर्वत्र ६ ३२
आदित्यानामहं विष्णुः १० २१
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् २ ७०
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः ८ १६
आयुधानामहं वज्रम् १० २८
आयुः सत्त्वबलारोग्य १७ ८
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् ६ ३
आवृतं ज्ञानमेतेन. ३ ३९
आशापाशशतैर्बद्धाः १६ १२
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम् २ २९
आसुरीं योनिमापन्नाः १६ २०
आहारस्त्वपि सर्वस्य . १७ ७
आहुस्त्वामृषयः सर्वे . १० १३
(इ)
इच्छाद्वेषसमुत्थेन....... ७ २७
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् . १३ ६
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम्. १३ १८
इति गुह्यतमं शास्त्रम् १५ २०
इति ते ज्ञानमाख्यातम्. १८ ६३
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा ११ ५०
इत्यहं वासुदेवस्य . १८ ७४
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य १४ २
इदं शरीरं कौन्तेय १३ १
इदं तु ते गुह्यतमम् ९ १
इदं ते नातपस्काय. १८ ६७
इदमद्य मया लब्धम् १६ १३
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे . ३ ३४
इन्द्रियाणां हि चरताम् २ ६७
इन्द्रियाणि पराण्याहुः ३ ४२
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः ३ ४०
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् १३ ८
इमं विवस्वते योगम् ४ १
इष्टान्भोगान्हि वो देवाः . ३ १२
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नम्. ११ ७
इहैव तैर्जितः सर्गः ५ १९
(ई)
ईश्वरः सर्वभूतानाम्. १८ ६१
(उ)
उच्चैःश्रवसमश्वानाम् १० २७
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि १५ १०
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः १५ १७
उत्सन्नकुलधर्माणाम् . १ ४४
उत्सीदेयुरिमे लोकाः. ३ २४
उदाराः सर्व एवैते ७ १८
उदासीनवदासीनः . १४ २३
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानम् ६ ५
उपद्रष्टानुमन्ता च १३ २२
(ऊ)
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः १४ १८
ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् १५ १
(ऋ)
ऋषिभिर्बहुधा गीतम् १३ ४
(ए)
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य ११ ३५
एतद्योनीनि भूतानि ७ ६
एतन्मे संशयं कृष्ण ६ ३९
एतां दृष्टिमवष्टभ्य १६ ९
एतान्न हन्तुमिच्छामि. . १ ३५
एतां विभूतिं योगं च १० ७
एतान्यपि तु कर्माणि १८ ६
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय १६ २२
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म ४ १५
एवं परम्परा प्राप्तम् ४ २
एवं प्रवर्तितं चक्रम् ३ १६
एवं बहुविधा यज्ञा ४ ३२
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा ३ ४३
एवं सततयुक्ता ये . १२ १
एवमुक्तो हृषीकेशः १ २४
एवमुक्त्वा ततो राजन्. ११ ९
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये १ ४७
एवमुक्त्वा हृषीकेशम् २ ९
एवमेतद्यथात्थ त्वम् ११ ३
एषा तेऽभिहिता सांख्ये. २ ३९
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ २ ७२
(ओ)
ॐ तत्सदिति निर्देशः . १७ २३
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म . ८ १३
(क)
कच्चिदेतच्छुतं पार्थ १८ ७२
कच्चिन्नोभयविभ्रष्टः ६ ३८
कट्द्वम्ललवणात्युष्ण- १७ ९
कथं न ज्ञेयमस्माभिः १ ३९
कथं भीष्ममहं संख्ये. २ ४
कथं विद्यामहं योगिन्. १० १७
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि. २ ५१
कर्मणैव हि संसिद्धिम् ३ २०
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् . ४ १७
कर्मणः सुकृतस्याहुः १४ १६
कर्मण्यकर्म यः पश्येत् ४ १८
कर्मण्येवाधिकारस्ते २ ४७
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि. ३ १५
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य. ३ ६
कर्षयन्तः शरीरस्थम् १७ ६
कविं पुराणमनुशासितारम् ८ ९
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् ११ ३७
काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिम्. ४ १२
काम एष क्रोध एष . ३ ३७
कामक्रोधवियुक्तानाम् ५ २६
काममाश्रित्य दुष्करम् १६ १०
कामात्मानः स्वर्गपराः २ ४३
कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः . ७ २०
काम्यानां कर्मणां न्यासम्. १८ २
कायेन मनसा बुद्धया ५ ११
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः २ ७
कार्यकारणकर्तृत्वे १३ २०
कार्यमित्येव यत्कर्म १८ ९
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः ११ ३२
काश्यश्च परमेष्वासः . १ १७
किं कर्म किमकर्मेति. ४ १६
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् ८ १
किं पुनर्बाह्मणाः पुण्याः ९ ३३
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् ११ ४६
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च ११ १७
कुतस्त्वा कश्मलमिदम् . २ २
कुलक्षये प्रणश्यन्ति १ ४०
कृपया परयाऽऽविष्टः. १ २८
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यम् . १८ ४४
कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतान्. १४ २१
क्रोधाद्भवति सम्मोहः २ ६३
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् १२ ५
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ २ ३
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ९ ३१
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् १३ ३४
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि. १३ २
(ग)
तसङ्गस्य मुक्तस्य ४ २३
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी ९ १८
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् . १ ३०
गामाविश्य च भूतानि . १५ १३
गुणानेतानतीत्य त्रीन् . १४ २०
गुरूनहत्वा हि महानुभावान् २ ५
(च)
चञ्चलं हि मनः कृष्ण ६ ३४
चतुर्विधा भजन्ते माम् ७ १६
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम् ४ १३
चिन्तामपरिमेयां च. १६ ११
चेतसा सर्वकर्माणि. १८ ५७
(ज)
जन्म कर्म च मे दिव्यम्. ४ ९
जरामरणमोक्षाय . . ७ २९
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः . २ २७
जितात्मनः प्रशान्तस्य ६ ७
ज्ञानं कर्म च कर्ता च. १८ १९
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता. १८ १८
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् ७ २
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ९ १५
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ६ ८
ज्ञानेन तु तदज्ञानम् ५ १६
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि १३ १२
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी ५ ३
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते ३ १
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः . १३ १७
(त)
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य १८ ७७
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च १३ ३
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् १५ ४
ततः शंखाश्च भेर्यश्च १ १३
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते. १ १४
ततः स विस्मयाविष्टः ११ १४
तत्त्ववित्तु महाबाहो ३ २८
तत्र तं बुद्धिसंयोगम् . . ६ ४३
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्. १४ ६
तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः १ २६
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् ११ १३
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा. ६ १२
तत्रैवं सति कर्तारम् १८ १६
तदित्यनभिसन्धाय . १७ २५
तद्बुद्धयस्तदात्मानः . ५ १७
तद्विद्धि प्रणिपातेन ४ ३४
तपस्विभ्योऽधिको योगी ६ ४६
तपाम्यहमहं वर्षम् ९ १९
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि १४ ८
तमुवाच हृषीकेशः २ १०
तमेव शरणं गच्छ . १८ ६२
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते १६ २४
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ ३ ४१
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व ११ ३३
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायम् . ११ ४४
तस्मात्सर्वेषु कालेषु . ८ ७
तस्मादज्ञानसंभूतम् ४ ४२
तस्मादसक्तः सततम्. ३ १९
तस्मादोमित्युदाहृत्य १७ २४
तस्माद्यस्य महाबाहो. २ ६८
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् १ ३७
तस्य संजनयन्हर्षम् . १ १२
तानहं द्विषतः क्रूरान् १६ १९
तानि सर्वाणि संयम्य २ ६१
तुल्यनिन्दास्तुतिमाँनी . १२ १९
तेजः क्षमा धृतिः शौचम् . १६ ३
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् ९ २१
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः ७ १७
तेषां सततयुक्तानाम् १० १०
तेषामहं समुद्धर्ता १२ ७
तेषामेवानुकम्पार्थम् १० ११
तं तथा कृपयाऽऽविष्टम् २ १
तं विद्यादुःखसंयोग. ६ २३
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्. ४ २०
त्याज्यं दोषवदित्येके १८ ३
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः ७ १३
त्रिविधा भवति श्रद्धा १७ २
त्रिविधं नरकस्येदम् १६ २१
त्रैगुण्यविषया वेदाः २ ४५
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः ९ २०
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् . ११ १८
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः ११ ३८
(द)
दण्डो दमयतामस्मि १० ३८
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च १६ ४
दातव्यमिति यद्दानम् १६ २०
दिवि सूर्यसहस्रस्य ११ १२
दिव्यमाल्याम्बरधरम् ११ ११
दुःखमित्येव यत्कर्म १८ ८
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः २ ५६
दूरेण ह्यवरं कर्म २ ४९
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् . १ २
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम् ११ ५१
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् . १७ १४
देवान्भावयतानेन . ३ ११
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे २ १३
देही नित्यमवध्योऽयम् २ ३०
दैवमेवापरे यज्ञम्. ४ २५
दैवी संपद्विमोक्षाय. १६ ५
दैवी ह्येषा गुणमयी ७ १४
दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् १ ४३
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि. ११ २५
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि. ११ २०
द्यूतं छलयतामस्मि. १० ३६
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा ४ २८
दुपदो द्रौपदेयाश्च. १ १८
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च. ११ ३४
द्वाविमौ पुरुषौ लोके १५ १६
द्वौ भूतसगौं लोकेऽस्मिन् . १६ ६
(ध)
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे १ १
धूमेनाव्रियते वह्निः ३ ३८
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः ८ २५
धृत्या यया धारयते १८ ३३
धृष्टकेतुश्चेकितानः. १ ५
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति. १३ २४
ध्यायतो विषयान्पुंस. २ ६२
(न)
न कर्तृत्वं न कर्माणि ५ १४
न कर्मणामनारम्भात्. ३ ४
न काङ्क्ष विजयं कृष्ण. १ ३२
न च तस्मान्मनुष्येषु १८ ६९
न च मत्स्थानि भूतानि . ९ ५
न च मां तानि कर्माणि ९ ९
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः २ ६
न जायते प्रियते वा कदाचित् . २ २०
न तदस्ति पृथिव्यां वा १८ ४०
न तद्भासयते सूर्यः. १५ ६
न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् ११ ८
न त्वेवाहं जातु नासम् २ १२
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म १८ १०
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य. ५ २०
न बुद्धिभेदं जनयेत् ३ २६
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्. ११ २४
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते. ११ ४०
न मां कर्माणि लिम्पन्ति ४ १४
न मां दुष्कृतिनो मूढाः . ७ १५
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् ३ २२
न मे विदुः सुरगणाः १० २
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते १५ ३
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः ११ ४८
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा १८ ७३
न हि कश्चित्क्षणमपि. ३ ५
न हि ज्ञानेन सदृशम्. ४ ३८
न हि देहभृता शक्यम्. १८ ११
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् . २ ८
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति. ६ १६
नादत्ते कस्यचित्पापम् ५ १५
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम् १० ४०
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् १४ १९
नासतो विद्यते भावो. २ १६
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य. २ ६६
नाहं प्रकाशः सर्वस्य. ७ २५
नाहं वेदैर्न तपसा ११ ५३
निमित्तानि च पश्यामि १ ३१
नियतं कुरु कर्म त्वम् ………………………………. ३ ८
नियतं सङ्गरर्हितम् ………………………………. १८ २३
नियतस्य तु संन्यासः………………………………. १८ ७
निराशीर्यतचित्तात्मा .………………………………. ४ २१
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः ………………………………. १५ ५
निश्चयं शृणु मे तत्र...………………………………. १८ ४
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः ………………………………. १ ३६
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति ………………………………. २ ४०
नैते सृती पार्थ जानन् ………………………………. ८ २७
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि ………………………………. २ २३
नैव किंचित्करोमीति.………………………………. ५ ८
नैव तस्य कृतेनार्थः ………………………………. ३ १८
(प)
पञ्चैतानि महाबाहो .………………………………. १८ १३
पत्रं पुष्पं फलं तोयम् ………………………………. ९ २६
परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः ………………………………. ८ २०
परित्राणाय साधूनाम्. ………………………………. ४ ८
परं ब्रह्म परं धाम ………………………………. १० १२२
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ………………………………. १४ १
पवनः पवतामस्मि.………………………………. १० ३१
पश्य मे पार्थ रूपाणि ………………………………. ११ ५
पश्यादित्यान्वसून्रुद्रान्.………………………………. ११ ६
पश्यामि देवांस्तव देव देहे ………………………………. ११ १५
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् ………………………………. १ ३
पाञ्चजन्यं हृषीकेशः .………………………………. १ १५
पार्थ नैवेह नामुत्र.………………………………. ६ ४०
पितासि लोकस्य चराचरस्य ………………………………. ११ ४३
पिताऽहमस्य जगतः .………………………………. ९ १७
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च ………………………………. ७ ९
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि ………………………………. १३ २१
पुरुषः स परः पार्थ ………………………………. ८ २२
पुरोधसां च मुख्यं माम् ………………………………. १० २४
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ………………………………. ६ ४४
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् ………………………………. १८ २१
प्रकाशं च प्रवृतिं च ………………………………. १४ २२
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी ………………………………. १३ १९
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य. ………………………………. ९ १८
प्रकृतेः क्रियमाणानि .………………………………. ३ २७
प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः ………………………………. ३ २९
प्रकृत्यैव च कर्माणि ………………………………. १३ २९
प्रजहाति यदा कामान् ………………………………. २ ५५
प्रयत्नाद्यतमानस्तु ………………………………. ६ ४५
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन ………………………………. ८ १०
प्रलपन्विसृजन्गृह्णन् .………………………………. ५ ९
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः ………………………………. १६ ७
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये ………………………………. १८ ३०
प्रशान्तमनसं ह्येनम्………………………………. ६ २७
प्रशान्तात्मा विगतभीः………………………………. ६ १४
प्रसादे सर्वदुःखानाम्. ………………………………. २ ६५
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् ………………………………. १० ३०
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् ………………………………. ६ ४१
(ब)
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य.………………………………. ६ ६
बलं बलवताम् ………………………………. ७ ११
बहिरन्तश्च भूतानाम् ………………………………. १३ १५
बहूनां जन्मनामन्ते ………………………………. ७ ११
बहूनि मे व्यतीतानि . ………………………………. ४ ५
बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा ………………………………. ५ २१
बीजं मां सर्वभूतानाम् ………………………………. ७ १०
बुद्धियुक्तो जहातीह ………………………………. २ ५०
बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः………………………………. १० ४
बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव ………………………………. १८ २१
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः………………………………. १८ ५१
बृहत्साम तथा साम्नाम् ………………………………. १० ३५
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्. ………………………………. १४ २७
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ………………………………. ५ १०
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ………………………………. १८ ५४
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ………………………………. ४ २४
ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् ………………………………. १८ २१
(भ)
भक्त्या त्वनन्यया शक्यः.………………………………. ११ ५४
भक्त्या मामभिजानाति ………………………………. १८ ५५
भयाद्रणादुपरतम् .………………………………. २ ३५
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च.………………………………. १ ८
भवाप्ययौ हि भूतानाम् ………………………………. ११ २
भीष्मद्रोणप्रमुखतः ………………………………. १ २५
भूतग्रामः स एवायम्.………………………………. ८ १९
भूमिरापोऽनलो वायुः ………………………………. ७ ४
भूय एव महाबाहो .………………………………. १० १
भोक्तारं यज्ञतपसाम्.………………………………. ५ २९
भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् .………………………………. २ ४४
(म)
मच्चित्ता मद्रतप्राणाः ………………………………. १० ९
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि ………………………………. १८ ५८
मत्कर्मकृन्मत्परमः .………………………………. ११ ५५
मत्तः परतरं नान्यत् .………………………………. ७ ७
मदनुग्रहाय परमम् ………………………………. ११ १
मनःप्रसादः सौम्यत्वम्.………………………………. १७ १६
मनुष्याणां सहस्रेषु ………………………………. ७ ३
मन्मना भव मद्भक्तः ………………………………. १८ ६५
मन्मना भव मद्भक्तः ………………………………. ९ ३४
मन्यसे यदि तच्छक्यम् ………………………………. ११ ४
मम योनिर्महद्ब्रह्म .………………………………. १४ ३
ममैवांशो जीवलोके ………………………………. १५ ७
मया ततमिदं सर्वम् .………………………………. ९ ४
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः. ………………………………. ९ १०
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् .………………………………. ११ ४७
मयि चानन्ययोगेन. ………………………………. १३ १०
मयि सर्वाणि कर्माणि ………………………………. ३ ३०
मय्यावेश्य मनो ये माम् ………………………………. १२ २
मय्यासक्तमनाः पार्थ ………………………………. ७ १
मय्येव मन आधत्स्व ………………………………. १२ ८
महर्षयः सप्त पूर्वे ………………………………. १० ६
महर्षीणां भृगुरहम् . ………………………………. १० २५
महात्मानस्तु मां पार्थ ………………………………. ९ १३
महाभूतान्यहंकारः ………………………………. १३ ५
मा ते व्यथा मा च विमूढभावः ………………………………. ११ ४९
मां च योऽव्यभिचारेण. ………………………………. १४ २६
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य . ………………………………. ९ ३२
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय ………………………………. २ १४
मानापमानयोस्तुल्यः ………………………………. १४ २५
मामुपेत्य पुनर्जन्म ………………………………. ८ १५
मुक्तसङ्गोऽनहंवादी. ………………………………. १८ २६
मूढग्राहेणात्मनो यत् ………………………………. १७ १९
मृत्युः सर्वहरश्चाहम् ………………………………. १० ३४
मोघाशा मोघकर्माणः ………………………………. ९ १२
(य)
य इमं परमं गुह्यम्. ………………………………. १८ ६८
य एनं वेत्ति हन्तारम्. ………………………………. . २ १९
य एवं वेत्ति पुरुषम् ………………………………. १३ २३
यं यं वाऽपि स्मरन्भावम् ………………………………. ८ ६
यं लब्ध्वा चापरं लाभम् ………………………………. ६ २२
यं संन्यासमिति प्राहुः ………………………………. ६ २
यं हि न व्यथयन्त्येते ………………………………. २ १५
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य.………………………………. १६ २३
यः सर्वत्रानभिस्नेहः ………………………………. २ ५७
यच्चापि सर्वभूतानाम् ………………………………. १० ३९
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि ………………………………. ११ ४२
यजन्ते सात्त्विका देवान् ………………………………. १७ ४
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् ………………………………. ४ ३५
यज्ञदानतपःकर्म.………………………………. १८ ५
यज्ञशिष्टामृतभुजः. ………………………………. ४ ३१
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः.………………………………. ३ १३
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र.………………………………. ३ ९
यज्ञे तपसि दाने च.………………………………. १७ २७
यततो ह्यपि कौन्तेय.………………………………. २ ६०
यतन्तो योगिनश्चैनम् ………………………………. १५ ११
यतः प्रवत्तिर्भूतानाम् ………………………………. १८ ४६
यत्करोषि यदश्नासि .………………………………. ९ २७
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम्.………………………………. ५ ५
यतेन्द्रियमनोबुद्धिः ………………………………. ५ २८
यतो यतो निश्चरति .………………………………. ६ २६
यत्तदग्रे विषमिव………………………………. १८ ३७
यत्तु कामेप्सुना कर्म ………………………………. १८ २४
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्.………………………………. १८ २२
यत्तु प्रत्युपकारार्थम् ………………………………. १७ २१
यत्र काले त्वनावृत्तिम् ………………………………. ८ २३
यत्र योगेश्वरः कृष्णः ………………………………. १८ ७८
यत्रोपरमते चित्तम् ………………………………. ६ २०
यथाकाशस्थितो नित्यम्.………………………………. ९ ६
यथा दीपो निवातस्थः ………………………………. ६ १९
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः .………………………………. ११ २८
यथा प्रकाशयत्येकः ………………………………. १३ ३३
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः ………………………………. ११ २९
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् ………………………………. १३ ३२
यथैधांसि समिद्धोऽग्निः .………………………………. ४ ३७
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति. ………………………………. ८ ११
यदग्रे चानुबन्धे च. ………………………………. १८ ३९
यदहंकारमाश्रित्य ………………………………. १८ ५९
यदा ते मोहकलिलम् ………………………………. २ ५२
यदादित्यगतं तेजः . ………………………………. १५ १२
यदा भूतपृथग्भावम् ………………………………. १३ ३०
यदा यदा हि धर्मस्य. ………………………………. ४ ७
यदा विनियतं चित्तम् ………………………………. ६ १८
यदा संहरते चायम् ………………………………. २ ५८
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु ………………………………. १४ १४
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु ………………………………. ६ ४
यदि मामप्रतीकारम् ………………………………. १ ४६
यदि ह्यहं न वर्तेयम् .………………………………. ३ २३
यदृच्छया चोपपन्नम्. .………………………………. २ ३२
यदृच्छालाभसन्तुष्टः. .………………………………. ४ २२
यद्यदाचरति श्रेष्ठः. .………………………………. ३ २१
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् .………………………………. १० ४१
यद्यप्येते न पश्यन्ति . .………………………………. १ ३८
यया तु धर्मकामार्थान्. .………………………………. १८ ३४
यया धर्ममधर्मं च . .………………………………. १८ ३१
यया स्वप्नं भयं शोकम् .………………………………. १८ ३५
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् .………………………………. ३ १७
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा .………………………………. ३ ७
यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् . .………………………………. १५ १८
यस्मान्नोद्विजते लोकः . .………………………………. १२ १५
यस्य नाहंकृतो भावः .………………………………. १८ १७
यस्य सर्वे समारम्भाः .………………………………. ४ १९
यातयामं गतरसम् . .………………………………. १७ १०
या निशा सर्वभूतानाम् .………………………………. २ ६९
यान्ति देवव्रता देवान् .………………………………. ९ २५
यामिमां पुष्पितां वाचम्. .………………………………. २ ४२
यावत्सञ्जायते किश्चित् .………………………………. १३ २६
यावदेतान्निरीक्षेऽहम् . .………………………………. १ २२
यावानर्थ उदपाने . .………………………………. २ ४६
युक्ताहारविहारस्य .………………………………. ६ १७
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा .………………………………. ५ १२
युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियत- . .……………………… ६ १५
युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगत- .…………………………… ६ २८
युधामन्युश्च विक्रान्तः .………………………………. १ ६
ये चैव सात्त्विका भावाः .………………………………. ७ १२
ये तु धर्ष्यामृतमिदम् .………………………………. १२ २०
ये तु सर्वाणि कर्माणि. .………………………………. १२ ६
ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् .………………………………. १२ ३
ये त्वेतदभ्यसूयन्तः .………………………………. ३ ३२
येऽप्यन्यदेवता भक्ताः .………………………………. ९ २३
ये मे मतमिदं नित्यम् .………………………………. ३ ३१
ये यथा मां प्रपद्यन्ते . .………………………………. ४ ११
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य .………………………………. १७ १
येषां त्वन्तगतं पापम् .………………………………. ७ २८
येषामर्थे काङ्क्षितं नो .………………………………. १ ३३
ये हि संस्पर्शजा भोगाः . .………………………………. ५ २२
योगयुक्तो विशुद्धात्मा .………………………………. ५ ७
योगसंन्यस्तकर्माणम्. .………………………………. ४ ४१
योगस्थः कुरु कर्माणि .………………………………. २ ४८
योगिनामपि सर्वेषाम्. .………………………………. ६ ४७
योगी युञ्जीत सततम् .………………………………. ६ १०
योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् .………………………………. १ २३
यो न हृष्यति न द्वेष्टि. .………………………………. १२ १७
योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः .………………………………. ५ २४
यो मां पश्यति सर्वत्र .………………………………. ६ ३०
यो मामजमनादिं च .………………………………. १० ३
यो मामेवमसंमूढः .………………………………. १५ १९
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः .………………………………. ६ ३३
यो यो यां यां तनुं भक्तः .………………………………. ७ २१
(र)
रजसि प्रलयं गत्वा .………………………………. १४ १५
रजस्तमश्चाभिभूय .………………………………. १४ १०
रजो रागात्मकं विद्धि . .………………………………. १४ ७
रसोऽहमप्सु कौन्तेय . .………………………………. ७ ८
रागद्वेषवियुक्तैस्तु . .………………………………. २ ६४
रागी कर्मफलप्रेप्सुः .………………………………. १८ २७
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य . .………………………………. १८ ७६
राजविद्या राजगुह्यम्. .………………………………. ९ २
रुद्राणां शंकरश्चास्मि .………………………………. १० २३
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः .………………………………. ११ २२
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् . .………………………………. ११ २३
(ल)
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्. .………………………………. ५ २५
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात्. .………………………………. ११ ३०
लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा .………………………………. ३ ३
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः .………………………………. १४ १२
(व)
वक्तुमर्हस्यशेषेण .………………………………. १० १६
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति .………………………………. ११ २७
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः. .………………………………. ११ ३९
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय. .………………………………. २ २२
विद्याविनयसंपन्ने . .………………………………. ५ १८
विधिहीनमसृष्टान्नम् .………………………………. १७ १३
विविक्तसेवी लघ्वाशी .………………………………. १८ ५२
विषया विनिवर्तन्ते .………………………………. २ ५९
विषयेन्द्रियसंयोगात् .………………………………. १८ ३८
विस्तरेणात्मनो योगम्. .………………………………. १० १८
विहाय कामान्यः सर्वान् .………………………………. २ ७१
वीतरागभयक्रोधाः .………………………………. ४ १०
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि .………………………………. १० ३७
वेदानां सामवेदोऽस्मि . .………………………………. १० २२
वेदाविनाशिनं नित्यम् .………………………………. २ २१
वेदाहं समतीतानि .………………………………. ७ २६
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव . .………………………………. ८ २८
व्यवसायात्मिका बुद्धिः . .………………………………. २ ४१
व्यामिश्रेणेव वाक्येन. .………………………………. ३ २
व्यासप्रसादाच्छुतवान्. .………………………………. १८ ७५
(श)
शक्नोतीहैव यः सोढुम् . .………………………………. ५ २३
शनैः शनैरुपरमेत्. .………………………………. ६ २५
शमो दमस्तपः शौचम्. .………………………………. १८ ४२
शरीरं यदवाप्नोति . .………………………………. १५ ८
शरीरवाङ्मनोभिर्यत् .………………………………. १८ १५
शुक्लकृष्णे गती ह्येते .………………………………. ८ २६
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य. .………………………………. ६ ११
शुभाशुभफलैरेवम् .………………………………. ९ २८
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् .………………………………. १८ ४३
श्रद्धया परया तप्तम् .………………………………. १७ १७
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम् .………………………………. ४ ३९
श्रद्धावाननसूयश्च .………………………………. १८ ७१
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते .………………………………. २ ५३
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञात्. .………………………………. ४ ३३
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः .………………………………. ३ ३५
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः .………………………………. १८ ४७
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् .………………………………. १२ १२
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये . .………………………………. ४ २६
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च . .………………………………. १५ ९
श्वशुरान्सुहृदश्चैव .………………………………. १ २७
(स)
स एवायं मया तेऽद्य. .………………………………. ४ ३
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः . .………………………………. ३ २५
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्. .………………………………. ११ ४१
स घोषो धार्तराष्ट्राणाम्. .………………………………. १ १९
संकरो नरकायैव. .………………………………. १ ४२
संकल्पप्रभवान्कामान् .………………………………. ६ २४
संनियम्येन्द्रियग्रामम् .………………………………. १२ ४
सततं कीर्तयन्तो माम् .………………………………. ९ १४
स तया श्रद्धया युक्तः .………………………………. ७ २२
सत्कारमानपूजार्थम् .………………………………. १७ १८
सत्त्वं रजस्तम इति. .………………………………. १४ ५
सत्त्वं सुखे सञ्जयति .………………………………. १४ ९
सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्. .………………………………. १४ १७
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य .………………………………. १७ ३
सदृशं चेष्टते स्वस्याः . .………………………………. ३ ३३
सद्भावे साधुभावे च .………………………………. १७ २६
संतुष्टः सततं योगी .………………………………. १२ १४
संन्यासं कर्मणां कृष्ण .………………………………. ५ १
संन्यासः कर्मयोगश्च . . .………………………………. ५ २
संन्यासस्तु महाबाहो. .………………………………. ५ ६
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् . .………………………………. १८ १
समं कायशिरोग्रीवम्. .………………………………. ६ १३
समं पश्यन्हि सर्वत्र .………………………………. १३ २८
समं सर्वेषु भूतेषु .………………………………. १३ २७
समः शत्रौ च मित्रे च. .………………………………. १२ १८
समदुःखसुखः स्वस्थः. .………………………………. १४ २४
समोऽहं सर्वभूतेषु .………………………………. ९ २९
सर्गाणामादिरन्तश्च . .………………………………. १० ३२
सर्वकर्माणि मनसा .………………………………. ५ १३
सर्वकर्माण्यपि सदा .………………………………. १८ ५६
सर्वगुह्यतमं भूयः .………………………………. १८ ६४
सर्वतःपाणिपादं तत् .………………………………. १३ १३
सर्वद्वाराणि संयम्य .………………………………. ८ १२
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् .………………………………. १४ ११
सर्वधर्मान्परित्यज्य. .………………………………. १८ ६६
सर्वभूतस्थमात्मानम् . .………………………………. ६ २९
सर्वभूतस्थितं यो माम् .………………………………. ६ ३१
सर्वभूतानि कौन्तेय . .………………………………. ९ ७
सर्वभूतेषु येनैकम् .………………………………. १८ २०
सर्वमेतदृतं मन्ये .………………………………. १० १४
सर्वयोनिषु कौन्तेय. .………………………………. १४ ४
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः. .………………………………. १५ १५
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि . .………………………………. ४ २७
सर्वेन्द्रियगुणाभासम् .………………………………. १३ १४
सहजं कर्म कौन्तेय .………………………………. १८ ४८
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा . .………………………………. ३ १०
सहस्रयुगपर्यन्तम् . .………………………………. ८ १७
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः .………………………………. ५ ४
साधिभूताधिदैवं माम् .………………………………. ७ ३०
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म .………………………………. १८ ५०
सीदन्ति मम गात्राणि .………………………………. १ २९
सुखं त्विदानीं त्रिविधम् .………………………………. १८ ३६
सुखदुःखे समे कृत्वा .………………………………. २ ३८
सुखमात्यन्तिकम्. .………………………………. ६ २१
सुदुर्दर्शमिदं रूपम् . .………………………………. ११ ५२
सुहृन्मित्रार्युदासीन .………………………………. ६ ९
स्थाने हृषीकेश. .………………………………. ११ ३६
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा .………………………………. २ ५४
स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यान् .………………………………. ५ २७
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य . .………………………………. २ ३१
स्वभावजेन कौन्तेय .………………………………. १८ ६०
स्वयमेवात्मना . .………………………………. १० १५
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः . .………………………………. १८ ४५
(ह)
हतो वा प्राप्स्यसि .………………………………. २ ३७
हन्त ते कथयिष्यामि .………………………………. १० . १९
हृषीकेशं तदा वाक्यम् . .………………………………. १ २१
२. विषयानुक्रमणिका
१. अज्ञानी : बुद्धिमान् व्यक्ति किसी अज्ञानी को कर्म करने से रोके नहीं, प्रत्युत् उसमें भक्तिभाव
भरे-३/२६,२९ भाग्य ७/२०, २४, १६/२३
२. अर्जुन : शोकाभिव्यक्ति- १/२८,३६,२/४-८; वीरता के लिए उपदेश की प्रार्थना-२/२,३; भगवान्
से प्रार्थना-११/१५-३१, ३६-४६
३. अशुभ कर्म : अशुभ कर्मों के ३/३७-४०
४. अश्रद्धा : अश्रद्धा की निन्दा-१७/२८
५. आत्मा : आत्मा की प्रकृति-२/११-३०; मित्र और शत्रु- ६/५,६
६. आसुरी : आसुरी प्रकृति का वर्णन-७/१५; ९/११,१२, २४; १६/४,५,७-२०; १७/५,६
७. इन्द्रियाँ : इन्द्रियाँ और मन, उनका संयम-२/६०,६१,६७; ३/३४,४१,४३, ५/२३
८. उद्भव : उद्भव और लय, उनका क्रम-८/१८,१९ ;९/७,८, १० ; १४/३,४
९. ॐ तत् सत् : महिमा-१७/२३-२७
१०. कर्म : विश्लेषण-३/२७-२९; कर्म की अनिर्वचनीय प्रकृति-४/१६-१८; पाँच कारण-१८/१४;
प्रवृत्ति और आधार - १८/१८
११. कर्मयोग : प्रमुख नियम-२/३८,४७,४८; ३/३०; ५/८, ९;६/२:१६/२४:१८/६,११,१७,४९,५६, ५७;
महिमा और अनिवार्यता-२/४०, ३/४-९,१६,१९-२५ ; ४/१५,१८ ; ५/२,६,११-१३ ; ६/१ ; १८/१८-६० लाभ-२/५१ ; ४:३२ ; देवों को यज्ञ रूप में कर्मयोग-३/१०-१५ ; बन्धन में नहीं डालता -४/२०-२५,४१ ;५/३,१०
१२. क्षेत्र : वर्णन-१३/५,६
१३. गीता : एक श्लोकी -१८/७८
१४. गुणातीत : जिसने गुणों से मोक्ष पा लिया है। विशेषतायें- १४/२२-२५
१५. जीव : प्रकृति और कार्य-१५/७-९
१६. ज्ञान : ज्ञानी के लिए कोई कर्म शेष नहीं-३/१७, १८; महिमा-३/४२,४३; ४/९,१०,१९,३३, ३५-
३९; ५/१७,२९; १०/३, ७, १३/२८, २९,३४; १४/१,२; १५/१९; कैसे प्राप्त करें ४/३४, ३९; ५/१६; ७/२९; १०/१०,११ प्राप्ति कब सम्भव ४/३८; १३/३०; परिभाषा-१३/२, ७-११,२७; १५/१
१७. तपस् : त्रिविध-१७/१४-१६
१८. तमस् : विशेषतायें-१४/८,९,१०,१३,१५,१८; १७/४, १०,१३,१९,२२; १८/७,२२,२५, २८, ३२,३५, ३९
१९. त्याग : विशेषतायें -१८/२,५,९-११
२०. दृष्टि : समदृष्टि-६/२९-३२
२१. दैवी : दैवी प्रकृति-९/१३-१५; १०/८,९, १६/१ , ३,५
२२. धाम : परम धाम-८/२१; १५/६
२३.नरक : तीन द्वार (नरक के) -१६/२१
२४. निर्वाण : निर्वाण-प्राप्ति-२/७२; ५/२४-२६; E / 84 २७, २८; निर्वाण के योग्य कौन-१८/५१-५३;
महिमा-१८/५४
२५. पथ : अयन, द्विविध-८/२३-२७
२६. पुरुष : दो पुरुष-१५/१६,१७
२७. पूर्णता : पूर्णत्व-प्राप्ति में कठिनाई ७/३,१९; ११/४७, ४८,५२,५३; कैसे प्राप्त करें-८/७-१०, १४,
२२; ११/५४,५५; १३/१८,२३; १४/२६; १६/२२; आवश्यकता-१३/१५; पूर्णत्व से गुणातीत होना-१४/१९,२०; योग्य कौन- १५/५,११
२८. प्रकृति : आधीनता (श्रेष्ठता) -३/३३; १८/४०; द्विविध प्रकृति-७/४,५
२९. प्रकृति पुरुष : स्वभाव और कार्य-१३/१९-२२,२६
३०. प्रतिकार : नियम-४/२; ७/२१; ९/२५
३१. बन्धन : कारण-१४/५
३२. ब्रह्मन् : ज्ञान का विषय, वर्णन-१३/१२-१७
३३. भक्त : विभाग-७/१६-१८; भक्त कौन-७/२८; विशेषतायें-१२/१३-२०
३४. भक्ति : विधि-४/११; ६/४७; ९/२२ , २६-३०,३४; १८/५५,६५,६६; विरक्त भाव से भक्ति की
उपयोगिता-९/२३; शक्ति-९/३०-३२;
निराकार ब्रह्म की भक्ति की उपयोगिता १२:३-५
३५. भगवान् : भगवान् के उपदेशों की महिमा-३/३१; १५/२०; १८/६७,७१; सर्वस्व एवं परम,७/६,७;
९/४-६; ११/३२,३३; १५/१७,१८; १८/६१ ; उनसे घृणा करने वालों का भाग्य-३/३२; १६/१६,१९; सर्वज्ञ- ४/५ ७/२६; अवतरण-४/६-८; अकर्ता, अभोक्ता-४/१३, १४; ५/१४,१५; ९/९; १८/३१,३२ विभूतियाँ७/८-१२; ९/१६-१९,२४; १०/२, ४-६, २०-४२; १४/२७; १५/१२-१५; पक्षपात-रहित-९/२९; विश्वरूपदर्शन-११/५-१३
३६. भोग : दुःखयोनयः-५/२२
३७. मन : साम्यावस्था-५/१८-२०; ६/७-९ ; अनासक्ति-५/२१; संयम की विधि -६/३५, ३६
३८. मोक्ष : अमृतत्व, मुक्ति, निर्वाण-देखें पूर्णत्व ।
३९. मोह : (अज्ञान, भ्रम) कारण-५/१५; ७/१३; मोहरहित कैसे हों - ७/१४ शक्ति-७/२५,२७,
१५,१०,११; १८/१६
४०. मृत्यु : मृत्यु के समय विचार-२/७२; ७/३० ; ८/५, ६, १०,१२,१३
४१. यज्ञ : प्रकार-४/२५-३०; यज्ञ की आवश्यकता- ४/३१
४२. योग : परिभाषा-२/४८,५०; अवस्था-२/५३; बुद्धि, स्तुति-२/४९,५०; अभ्यास की आवश्यकता-
२/६६; ६/२३,४६; ८/२७,२८; ज्ञान और कर्म-योग विरोधी नहीं, समान रूप से फलदायी-५/२,४,५; सार रूप में -५/२७,२८; ६/४-१८; प्रमुख नियम ६/२; दो विधियाँ ६/३; योगक्रम विस्तार से- ६ /१० - १४,२४,२६ अभ्यास के लिए कौन योग्य-६/१६,१७; अभ्यास के स्तर-१२/९-१२; प्रकार - १३/२४,२५
४३. योगी : सांसारिक के विपरीत -२/ ६९
४४. योगभ्रष्ट : नियति-६/४०-४५
४५. रजस् : विशेषतायें-१४/७,९,१०,१२,१५-१८; १७/४,९,१२,१८,२१; १८/८,२१,२४,२७, ३१,३४,३८
४६. विषय : विचारों का प्रभाव-२/६२,६३
४७. वेद : कर्मकाण्ड, अस्तुत-२/४२-४४; ९/२०,२१; योग से निम्न-२/४५,४६
४८. वैराग्य : शर्त-२/५२
४९. शान्ति : अन्तःशान्ति के प्रभाव-२/६५; प्राप्ति के योग्य कौन-२/७०,७१
५० . सत्त्व : विशेषतायें -१४/६,९,१०,११,१४,१६-१८; १७/४,८,११,१७,२०; १८/९,२०,२३,२६,
३०,३३,३७
५१. सन्देह : शोक और पतन का कारण-४/४०; ९/३ ; ज्ञान द्वारा निवारण-४/४२
५२. संसार : संसार-वृक्ष का वर्णन-१५ /२३; इससे मुक्ति- १५/३,४
५३. समाधि : समाध्यावस्था का वर्णन-६/१९-२२; इन्द्रिय-विषय का अतिक्रमण-२/५९
५४. स्थितप्रज्ञ : विशेषतायें-२/५५-५८,६१,६४,६८
५५. स्वधर्म : स्तुति-२/३१-३७; ३/३५; १८/४५-५८; ब्राह्मणों का धर्म-१८/४२; क्षत्रिय-१८/४३;
वैश्य-१८/४४; शूद्र-१८/४४
५६. सृष्टिकर्ता : लोक,नश्वर-८/१६-१९
आरती
जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते ।
हरि-हिय-कमल-विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते ।।
कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि, कामासक्तिहरा ।
तत्त्वज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्म परा ।। जय...
निश्चल-भक्ति-विधायिनि, निर्मल मलहारी।
शरण-रहस्य-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी ।। जय...
राग-द्वेष-विदारिणि, कारिणि मोद सदा ।
भव-भय-हारिणि तारिणि, परमानन्दप्रदा ।। जय...
आसुरभाव-विनाशिनि, नाशिनि तम रजनी ।
दैवी सद्गुणदायिनि, हरि-रसिका सजनी ।। जय...
समता-त्याग सिखावनि, हरि मुख की बानी।
सकल शास्त्र की स्वामिनि, श्रुतियों की रानी ।। जय...
दया-सुधा बरसावनि, मातु ! कृपा कीजै।
हरि-पद-प्रेम दान कर, अपनो कर लीजै ।। जय…
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती
८ सितम्बर, १८८७ को सन्त अप्पय्य दीक्षितार तथा अन्य अनेक ख्याति प्राप्त विद्वानों के सुप्रसिद्ध परिवार में जन्म लेने वाले श्री स्वामी शिवानन्द जी में वेदान्त के अध्ययन एवं अभ्यास के लिए समर्पित जीवन जीने की तो स्वाभाविक एवं जन्मजात प्रवृत्ति थी ही, इसके साथ-साथ सबकी सेवा करने की उत्कण्ठा तथा समस्त मानव-जाति से एकत्व की भावना उनमें सहजात ही थी।
सेवा के प्रति तीव्र रुचि ने उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र की ओर उन्मुख कर दिया और जहाँ उनकी सेवा की सर्वाधिक आवश्यकता थी, उस ओर शीघ्र ही वे अभिमुख हो गये। मलाया ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। इससे पूर्व वह एक स्वास्थ्य-सम्बन्धी पत्रिका का सम्पादन कर रहे थे, जिसमें स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याओं पर विस्तृत रूप से लिखा करते थे। उन्होंने पाया कि लोगों को सही जानकारी की अत्यधिक आवश्यकता है, अतः सही जानकारी देना उनका लक्ष्य ही बन गया।
यह एक दैवी विधान एवं मानव-जाति पर भगवान् की कृपा ही थी कि देह-मन के इस चिकित्सक ने अपनी जीविका का त्याग करके, मानव की आत्मा के उपचारक होने के लिए त्यागमय जीवन को अपना लिया। १९२४ में वह ऋषिकेश में बस गये, यहाँ कठोर तपस्या की और एक महान् योगी, सन्त, मनीषी एवं जीवन्मुक्त महात्मा के रूप में उद्भासित हुए।
१९३२ में स्वामी शिवानन्द जी ने 'शिवानन्द आश्रम' की स्थापना की; १९३६ में 'द डिवाइन लाइफ सोसायटी' का जन्म हुआ; १९४८ में 'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी' का शुभारम्भ किया। लोगों को योग और वेदान्त में प्रशिक्षित करना तथा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना इनका लक्ष्य था। १९५० में स्वामी जी ने भारत और लंका का द्रुत-भ्रमण किया । १९५३ में स्वामी जी ने 'वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स' (विश्व धर्म सम्मेलन) आयोजित किया। स्वामी जी ३०० से अधिक ग्रन्थों के रचयिता हैं तथा समस्त विश्व में विभिन्न धर्मो, जातियों और मतों के लोग उनके शिष्य हैं। स्वामी जी की कृतियों का अध्ययन करना परम ज्ञान के स्रोत का पान करना है। १४ जुलाई, १९६३ को स्वामी जी महासमाधि में लीन हो गये।