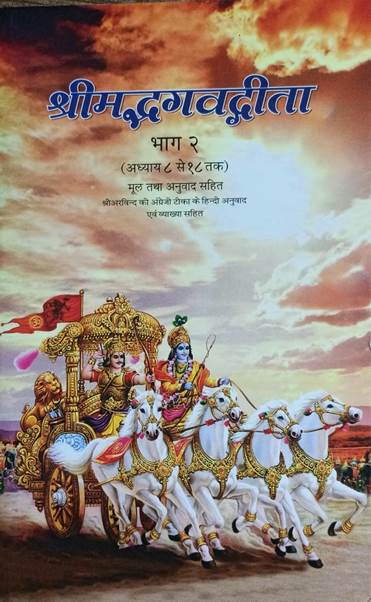
श्रीमद्भगवद्गीता
भाग २
अध्याय ८ से १८ तक
श्रीमद्भगवद्गीता
भाग २
(अध्याय ८ से १८ तक)
मूल तथा अनुवाद सहित
श्रीअरविन्द की अंग्रेजी टीका के हिन्दी अनुवाद एवं व्याख्या सहित
अंग्रेजी टीका का संपादन
स्व. श्री परमेश्वरी प्रसाद खेतान
हिन्दी व्याख्या
चन्द्र प्रकाश खेतान
हिन्दी अनुवाद व व्याख्या संपादन
पंकज बगड़िया
श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट झुंझुनू, राजस्थान
© श्रीअरविन्द आश्रम ट्रस्ट, २०१९
प्रकाशकः-
श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट
श्रीअरविन्द दिव्य जीवन आश्रम,
खेतान मोहल्ला
झुन्झुनू - ३३३००१, राजस्थान।
URL: www.sadlec.org www.resurgentindia.org
www.aurokart.com
मुद्रकः- श्रीअरविन्द आश्रम प्रेस
पुदुच्चेरी
भगवान् श्रीकृष्ण को समर्पित
जिनकी कृपा से हमें
श्रीअरविन्द व श्रीमाँ के चरण कमलों की
शरण प्राप्त हुई है।
संपादकीय नोट
यह पुस्तक स्वर्गीय श्री परमेश्वरी प्रसाद खेतान की अंग्रेजी पुस्तक 'द भगवद् गीता' के हिन्दी रूपांतर के आधार पर श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट में हुए अध्ययन सत्रों के दौरान साधकों के बीच चर्चा-परिचर्चा, सहज अंतःस्फूर्णा तथा श्री चन्द्र प्रकाश जी खेतान के निजी आध्यात्मिक अनुभवों आदि के माध्यम से हुई श्रीअरविन्द व श्रीमाँ के मूल शब्दों की व्याख्या का अभिलेख है। सत्रों के ध्वनिलेखों को भाषा में ढालने और उनकी एडिटिंग (संपादन), संशोधन आदि का कार्य सुश्री सुमन शर्मा व श्री दीपक तुलस्यान की सहायता से संपादक द्वारा किया गया है। अनेक स्थानों पर चर्चा-परिचर्चा के दौरान श्रीमाँ-श्रीअरविन्द तथा योगी श्रीकृष्णप्रेम के संदर्भों का उल्लेख किया गया जिन्हें कि यहाँ मूल रूप से सम्मिलित कर लिया गया है जो कि पाठक के लिये पूरे विषय को अधिक स्पष्ट, सुगम और प्रभावी बना देते हैं। व्याख्या को मूल से भिन्न करने के लिए तिरछे अक्षरों (italics) में दिया गया है। प्रथम भाग में गीता के प्रथम सात अध्यायों को सम्मिलित किया गया है और इस भाग में शेष ग्यारह अध्यायों को सम्मिलित किया गया है।
पुस्तक में प्रस्तुत गीता पर टीका श्रीमाँ की कृतियों से लिये कुछ संदर्भों को छोड़कर शेष श्रीअरविन्द के शब्दों में है जिनकी संदर्भ सूची अंत में दी जा रही है। विचार में निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर मूल संपादक श्री परमेश्वरी प्रसाद खेतान द्वारा कुछ शब्द या वाक्यांश जोड़े गए हैं जिन्हें वर्गाकार कोष्ठक में दिखाया गया है।
श्लोकों का अनुवाद तथा पुस्तक में दिये गये शीर्षक श्रीअरविन्द की पुस्तक 'ऐसेज ऑन द गीता' पर आधारित हैं। अध्यायों के परंपरागत शीर्षक प्रत्येक अध्याय के अंत में दिये गये हैं। हासिये में दी गई संख्याएँ गीता के अध्याय व श्लोक संख्या को दर्शाती हैं।
श्रीमाँ ने कहा है कि "श्रीअरविन्द गीता के संदेश को उस महान् आध्यात्मिक गति का आधार मानते हैं जो मानवजाति को अधिकाधिक उसकी मुक्ति की ओर, अर्थात् मिथ्यात्व और अज्ञान से निकलकर सत्य की ओर ले गई है, और आगे भी ले जाएगी। अपने प्रथम प्राकट्य के समय से ही गीता का अतिविशाल आध्यात्मिक प्रभाव रहा है; परंतु जो नवीन व्याख्या श्रीअरविन्द ने उसे प्रदान की है, उसके साथ ही उसकी प्रभावशालिता अत्यधिक
बढ़ गई है और निर्णायक बन गई है।"
वर्ष १९९२ में अपने प्रथम प्रकाशन के समय से ही 'द भगवद्गीता' पुस्तक को पाठकों द्वारा खूब सराहा गया है। श्रीअरविन्द की अद्भुत टीका के ऊपर अब इस व्याख्या के आने से हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक श्रीअरविन्द व श्रीमाँ के आलोक में गीता को समझने, उसे व्यावहारिक रूप से जीवन में उतारने में पाठकों के लिए सहायक सिद्ध होगी।
- पंकज बगड़िया
विषय-सूची
I. श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता और उनकी आध्यात्मिक यथार्थता
II. गीता तथा श्रीअरविन्द का संदेश
आठवाँ अध्याय
परम् ईश्वर
[सातवें अध्याय के अन्तिम दो श्लोकों में] कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द आये हैं जो अपने संक्षेप रूप में जगत् में परम् ईश्वर के' आविर्भाव के प्रधान मूलभूत सत्यों को देते हैं। सभी कारणसंबंधी या उत्पत्तिसंबंधी (originative) और कार्य या प्रभावसंबंधी (effective) तत्त्व इसमें विद्यमान हैं, वे सब तत्त्व विद्यमान हैं जिनसे अपने समग्र आत्मज्ञान की ओर लौटने में जीव को प्रयोजन है। सबसे पहले है 'तद्ब्रह्म; दूसरा है 'अध्यात्म' अर्थात् प्रकृति में आत्मसत्ता का तत्त्व; इसके बाद 'अधिभूत' और 'अधिदैव' अर्थात् सत्ता के बाह्य या वस्तुनिष्ठ भाव तथा आंतरिक अथवा आत्मनिष्ठ भाव; और अंत में है 'अधियज्ञ' अर्थात् कर्म और यज्ञ के वैश्विक तत्त्व का रहस्य। यहाँ श्रीकृष्ण के कहने का आशय यह है कि इन सबके ऊपर जो 'मैं' 'पुरुषोत्तम' हूँ, उस मुझको इन सब में होकर और इन सबके परस्पर सम्बन्धों के द्वारा ढूँढ़ना और जानना होगा (मां विदुः), - यही उस मानव चेतना के लिए एकमात्र पूर्ण मार्ग है जो कि मेरे पास लौट आने का पथ खोज रही है। परन्तु अपने-आप में ये पारिभाषिक शब्द शुरू में सर्वथा स्पष्ट नहीं होते या कम-से-कम ये भिन्न-भिन्न व्याख्याओं के लिए खुले होते हैं; इसलिए उनके वास्तविक अभिप्राय को सटीक-सुनिश्चित बनाने की आवश्यकता होती है और एकाएक ही शिष्य अर्जुन उनके स्पष्टीकरण की माँग कर बैठता है।
अर्जुन उवाच
किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ।। १।।
१. अर्जुन ने कहा : हे पुरुषोत्तमा तद् ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? और अधिभूत किसे कहा गया है, अधिदैव किसे कहा गया है?
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ।। २।।
२. हे मधुसूदना इस देह में अधियज्ञ क्या है? और भौतिक अस्तित्व से प्रयाण के संकटकाल में आत्मसंयत मनुष्य द्वारा किस प्रकार आप जाने जाते हो?
श्रीभगवान् उवाच
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ।। ३।।
३. श्रीभगवान् ने कहाः अक्षर परम् ब्रह्म है; स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं, सृजनात्मक प्रवृत्ति, विसर्ग; को कर्म की संज्ञा दी गई है जो समस्त भूतों को और उनके वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ भावों की उत्पत्ति करता है।
कृष्ण बहुत संक्षेप में इसका उत्तर देते हैं, - गीता कहीं भी किसी शुद्ध रूप से दार्शनिक व्याख्या पर बहुत अधिक देर तक नहीं ठहरती, वह उतनी ही बात और उसी ढंग से बतलाती है जो उनके सत्य को जीव के लिए ग्राह्य भर बना दे जो फिर तत्त्व को ग्रहण करके स्वानुभव की ओर आगे बढ़े। 'तद्ब्रह्म' से, जो कि ऐसा पद है जो उपनिषदों में लौकिक जीव के विपरीत ब्रह्मसत्ता या स्वयंभू सत्ता के लिए अनेक बार प्रयुक्त हुआ है, प्रतीत होता है कि गीता का अभिप्राय 'अक्षरं परमम्' अर्थात् उस अक्षर ब्रह्मसत्ता से है जो कि भगवान् की परम् आत्माभिव्यक्ति है और जिसकी अटल शाश्वतता पर शेष सभी कुछ, जो कुछ भी चल और विकसनशील है, आधारित है। अध्यात्म से इसका अभिप्राय है 'स्वभाव' अर्थात् परा प्रकृति में जीव की सत्ता का आत्मिक भाव और विधान। गीता कहती है कि 'कर्म' 'विसर्ग' का नाम है अर्थात् उस सृष्टि-प्रेरणा और शक्ति का जो इस आदि मूलगत 'स्वभाव' से सब चीजों को बाहर निकालती है और उस स्वभाव के ही प्रभाव से 'प्रकृति' में सब भूतों को उत्पत्ति, सृष्टि और पूर्णता साधित करती है।
यहाँ सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। गीता जिस 'अक्षरं परमम्' का यहाँ उल्लेख करती है वह वह अक्षर पुरुष नहीं है जिसकी हम पूर्व में चर्चा कर आए हैं। जिस अक्षर की यहाँ बात है वह तो वह परम् अविनाशी सत्ता है जिसे हम परंब्रह्म आदि की संज्ञाएँ देते हैं जो कि सभी कुछ का आधार है। अक्षर के बाद है 'स्वभाव'। हम पहले भी सतही भाव, स्वभाव और मद्भाव की चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक जीव के अंदर परा प्रकृति जिस विशिष्ट चीज की अभिव्यक्ति करना चाहती है वह उसका 'स्वभाव' है। हालाँकि बाहरी प्रकृति में जो अनेकानेक प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं वे इस स्वभाव से भिन्न हैं। परंतु व्यक्ति का जो सच्चा स्वभाव है, जिसके नियत कर्म किये जाने पर गीता बल देती है और जिस पर भारतीय संस्कृति में भी सदा ही बल दिया जाता रहा है, उसे ही 'अध्यात्म' कहते हैं। अध्यात्म के बाद आता है 'कर्म' अर्थात् सहज रूप से स्वभाव के द्वारा नियत की हुई मन, प्राण और शरीर की क्रियाएँ। कर्म केवल शरीर से ही नहीं किये जाते अपितु मानसिक क्रियाकलाप, प्राणिक भावनाएँ और आवेग आदि भी कर्म ही हैं। स्वभाव और स्वभाव नियत कर्म के विषय में तथा किस प्रकार भारतीय संस्कृति में उसके आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था आदि का निर्माण किया गया उसकी विशद चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं।
प्रश्न : धर्म क्या है?
उत्तर : धर्म तो बहुत सापेक्ष चीज है और यह व्यक्ति के आंतर्बाह्य विकास की अवस्था पर निर्भर करता है कि उसके लिए उपयुक्त धर्म क्या है। हालाँकि अंतर्निहित स्वभाव तो वही होगा परंतु विकास की अवस्था के अनुसार धर्म भिन्न-भिन्न होगा। ब्राह्मण के लिए एक प्रकार का धर्म है। परंतु उसी ब्राह्मण के लिए संकटकाल में धर्म बदल जाता है। इसलिए स्वभाव तो एक मूलभूत चीज है जिसका कि धर्म के द्वारा निरूपण करने का प्रयास किया जाता है क्योंकि धर्मों के द्वारा स्वभाव की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती इसीलिए गीता सभी धर्मों को त्याग देने और भगवान् की शरण ग्रहण करने का उपदेश करती है। पहले सभी प्रकार के ऊँचे से ऊँचे धर्मों का भी निरूपण करने के बाद, साधना, समर्पण, भक्ति आदि के धर्मों का भी निरूपण करने के बाद गीता इन सभी को छोड़कर भगवान् की शरण में जाने को कहती है। क्योंकि किसी भी धर्म के द्वारा व्यक्ति स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता। और 'मद्भाव' में तो व्यक्ति प्रभु के साथ एकत्व होने पर ही जा सकता है।
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्वाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ।। ४।।
४. हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन! अधिभूत क्षर भाव है, और अधिदैव पुरुष (प्रकृतिस्थ आत्मा) है; इस देह में यज्ञ, अधियज्ञ, का प्रभु मैं स्वयं ही हूँ।
'अधिभूत' से तात्पर्य है 'क्षर भाव' अर्थात् परिवर्तन की क्रिया के समस्त परिणाम। 'अधिदैव' से अभिप्रेत है पुरुष, प्रकृतिस्थ आत्मा अर्थात् वह आत्मनिष्ठ (subjective) सत्ता जो अपनी मूलसत्ता के समूचे क्षरभाव को, जो प्रकृति में कर्म के द्वारा साधित हुआ करता है, अपनी चेतना के विषय-रूप से देखता और भोग करता है। 'अधियज्ञ' से, भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि, 'मैं' स्वयं अभिप्रेत हूँ – 'मैं' अर्थात् अखिल कर्म और यज्ञ के प्रभु, भगवान् परमेश्वर, पुरुषोत्तम जो यहाँ इन सब देहधारियों के शरीर में गुप्त रूप से विराजमान हैं। अतः जो कुछ है सब इसी एक सूत्र में आ जाता है।
....यहाँ जगत् की प्रणाली (विसर्ग) के संबंध में गीता का भाव दर्शाया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम ब्रह्म अर्थात् परम् अक्षर स्वतःसिद्ध ब्रह्मसत्ता है; देश, काल और निमित्त में होनेवाले विश्वप्रकृति के खेल के पीछे सभी भूत यह ब्रह्म ही हैं। क्योंकि उस ब्रह्मसत्ता से ही देश, काल और निमित्त अस्तित्वमान रह पाते हैं और उस अपरिवर्तनीय सर्वव्यापी परन्तु फिर भी अविभाज्य आश्रय के बिना देश, काल और निमित्त अपने विभाग, परिणाम और मान निर्माण करने में प्रवृत्त नहीं हो सकते। परन्तु अक्षर ब्रह्म स्वयं कुछ नहीं करता, किसी कार्य का कारण नहीं होता, किसी बात का विधान नहीं करता; वह निष्पक्ष, सम और सर्वालंबनकारी है, परंतु वह चुनाव या आरम्भ नहीं करता। तो फिर वह क्या है जो उत्पन्न करता है, विधान करता है, और परम् प्रभु की वह दिव्य प्रेरणा प्रदान करता है? वह क्या है जो कर्म का नियामक है और जो शाश्वत सत्ता में से 'काल' के अन्दर इस विश्वलीला को सक्रिय रूप से प्रकट करता है? यह 'स्वभाव' रूप से प्रकृति है। परम्, परमेश्वर, पुरुषोत्तम अपनी सत्ता से उपस्थित हैं और वे ही अपनी सनातन अक्षर सत्ता के आधार पर अपनी परा आत्मशक्ति के कार्य को धारण करते हैं। वे अपनी भागवती सत्ता, चेतना, संकल्प या शक्ति को प्रकट करते हैं, ययेदं धार्यते जगत्: वही परा प्रकृति है। इस परा प्रकृति के अंदर आत्मा की आत्मचेतना, आत्मज्ञान के प्रकाश में गतिशील या ऊर्जस्वी विचार को, वह जिस किसी भी चीज को अपनी सत्ता में अलग करती है और उसे स्वभाव - अर्थात् जीव की आध्यात्मिक प्रकृति - में अभिव्यक्त करती है, उसके यथार्थ सत्य को देखती है। जो प्रत्येक जीव का अंतर्निहित सत्य और आत्मतत्त्व है, जो अपने-आप को अभिव्यक्ति में लाता है, जो सबके अंदर निहित वह मूलभूत भागवत् प्रकृति है जो सब प्रकार के परिवर्तनों, विपर्ययों और पुनरावर्तनों के पीछे सदा बनी रहती है, वही स्वभाव है। स्वभाव में जो कुछ है वह उसमें से विश्व-प्रकृति में छोड़ दिया जाता है ताकि विश्वप्रकृति पुरुषोत्तम की आंतरिक दृष्टि की देख-रेख में उससे जो कर सकती हो करे। इस सतत् स्वभाव में से, प्रत्येक संभूति की मूल प्रकृति और उसके मूल आत्मतत्त्व में से भिन्न-भिन्न भेदों का निर्माण करके यह विश्वप्रकृति उसके द्वारा उस स्वभाव को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है। वह अपने इन सब परिवर्तनों को नाम और रूप, काल और देश तथा देश-काल के अन्दर एक अवस्था से दूसरी अवस्था के उत्पन्न होने का जो क्रम है जिसे हम लोग कारणता, 'निमित्त', कहते हैं, उसे खोलकर प्रकट किया करती है।
अतः, वास्तव में तो कोई कार्य-कारण नहीं है। मूलभूत कारण तो केवल जगदम्बा का संकल्प है बाकी सब तो निमित्त ही है। उदाहरण के लिए यदि हमें अमुक जगह जाना हो तो जो भी मार्ग उसके लिए हम अपनाते हैं वे निमित्त बन जाते हैं। परंतु हम उस मार्ग विशेष से बाध्य नहीं हो जाते बल्कि दूसरे मार्ग भी अपना सकते हैं। वैसे ही यदि हमें बैठना हो तो हम किसी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वह कुर्सी निमित्त बन गई। इसमें भी हम किसी कुर्सी विशेष पर बैठने को बाध्य नहीं हैं। इसी प्रकार भागवती प्रकृति का संकल्प ही है जो मूल कारण है और अपनी अभिव्यक्ति के लिए वह जिन साधनों और माध्यमों को काम में लेती हैं वे सब निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए भगवान् अर्जुन को कहते हैं 'निमित्तमात्रं भव' क्योंकि जो होना है वह तो भागवती शक्ति द्वारा पहले ही किया जा चुका है। अर्जुन को तो उसका केवल निमित्त बनना है। और यदि वह सहर्ष निमित्त नहीं बनता तो या तो किसी अन्य को निमित्त बना लिया जाएगा या फिर परिस्थितियों की बाध्यकारी शक्ति के द्वारा अवश रूप से उसे ही निमित्त बनना पड़ेगा परंतु, भगवान् कहते हैं कि, ऐसा करने में कोई आध्यात्मिक श्रेय नहीं होता। कहने का अर्थ है कि निमित्त अपने आप में उस क्रिया का कारण नहीं है। यह कहना अयुक्तियुक्त होगा कि किसी मार्ग के कारण व्यक्ति किसी अमुक स्थान पर जाएगा या फिर किसी कुर्सी के कारण वह बैठेगा या फिर किसी साधन के कारण कोई कार्य करेगा। साधन को तो वह अपने कार्य के संकल्प को पूरा करने के लिए काम में ले सकता है।
xi.33
यहाँ स्वभाव के संबंध में जो बातें आईं हैं उनका इससे पहले गीता में निरूपण नहीं हुआ था। हमारे कर्म की नियामक बाहरी प्रकृति नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कभी भी दूसरे लोगों की इच्छा अथवा अन्य कोई बाहरी कारण नहीं होते। वास्तव में तो व्यक्ति के साथ जो कुछ भी घटित होता है वह उसके स्वभाव के अनुसार ही होता है। क्योंकि भले ही बाहरी रूप से मनुष्यों के अंदर कुछ चीजें समान हों परंतु प्रत्येक मनुष्य अपने अलग आत्मनिष्ठ जगत् में निवास करता है। हालाँकि अन्तरात्मा में सभी एक हैं परंतु स्वभाव में सभी का पृथक् गठन होने के कारण सभी अपने अलग ही जगत् में निवास करते हैं। प्रकृति भी हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति के अनुसार कार्य करती है। अपने आप में बाहरी प्रकृति हमारा कुछ नहीं कर सकती। और हमारे लिए कर्म भी तभी लाभकारी होते हैं जब वे स्वभाव के अनुकूल हों अर्थात् स्वभाव नियत कर्म हों। उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी रोगी के लिए दवाई लाने बाजार जाए तो उसका कर्म स्वभाव नियत तब होगा जब वह सही जगह जाकर और सही दवाई लेकर आए। वहीं, यदि वह बाजार की चकाचौंध में ही मुग्ध हो जाए या फिर किसी परिचित से निरर्थक बातचीत में लग जाए या फिर अन्य किसी ऐसे काम में लग जाए जो उसके लक्ष्य के प्रतिकूल हो, तो यह कर्म लाभकारी या उचित नहीं हुआ। इसीलिए स्वभाव नियत कर्म पर गीता इतना अधिक बल देती है और हमारी संस्कृति में भी इस पर अतिशय बल दिया जाता रहा है, क्योंकि स्वभाव नियत कर्म के द्वारा व्यक्ति सीधे उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है जिसके लिए वह इस अभिव्यक्ति में आया है। परंतु हमारे वर्तमान अज्ञानमय और अवचेतन जीवन में हमें अपने स्वभाव का सचेतन बोध ही नहीं होता इसलिए हमारे कर्म सचेतन रूप से उसके अनुकूल नहीं होते। इस चीज की गंभीरता को समझते हुए ही हमारी संस्कृति में हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की अपरिहार्यता अनुभव की जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र उसके स्वभाव के प्रति सचेतन बना दिया जाए और साथ ही उसके अनुकूल कर्म करने की सहायता प्रदान की जाए ताकि वह अपने सच्चे स्वभाव को अधिकाधिक अभिव्यक्त कर सके जिसके लिए कि वह इस अभिव्यक्ति में आया है।
वास्तव में तो परा प्रकृति ही स्वभाव रूप से जीव में विराजमान हैं और वे ही उसे उसके स्वभाव के अनुरूप आगे ले जा रही हैं परंतु अचेतन रूप से आगे बढ़ने में कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए हमारी संस्कृति का सदा ही सारा प्रयास इस ओर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यथाशीघ्र अपने स्वभाव को जान जाए और सचेतन रूप से उसकी ओर आगे बढ़े। और वास्तव में तो व्यक्ति को अपने स्वभाव का पता ही भगवान् की सीधी प्रेरणा से या फिर सद्गुरु के प्राप्त होने पर चलता है। और जब व्यक्ति अपने स्वभाव के प्रति, अपने अंदर जो परमात्मा का अंश है उसके प्रति सचेतन हो जाता है तब वह अपने कर्म उसकी अभिव्यक्ति के अनुरूप करता है। अन्यथा तो वह सदा ही शंकित रहता है कि कहीं उसके कर्म गुणों से प्रभावित तो नहीं हैं। और जब तक उसके कर्म गुणों से प्रभावित रहते हैं तब तक स्वभाव नियत कर्म नहीं किये जा सकते।
प्रश्न : हम कहते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के प्रति सचेतन होना होगा और अपने सतही भाव से स्वभाव की ओर जाना होगा। परंतु यह बाहरी भाव भी तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो इसका क्या औचित्य है कि वे इस सतही भाव को केवल इससे बाहर निकलने के लिये ही हमारे ऊपर लादते हैं?
उत्तर : वास्तव में तो किसी चीज का क्या औचित्य है यह तो सच्चे रूप से केवल परमात्मा ही जानते हैं। परंतु अवश्य ही पहले तो यह कहना अयुक्तियुक्त है कि परमात्मा हमारे ऊपर इस सतही प्रकृति या भाव को लादते हैं क्योंकि यदि वे ऐसा करते हों तो ऐसा वे स्वयं अपने आप के साथ ही तो करते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता तो है ही नहीं। केवल अहंबोध के कारण ही हमें यह तथ्य दिखाई नहीं देता। दूसरे, यह कहना भी असंगत बात है कि चूंकि परमात्मा ने ही यह माया फैलायी है अतः हमें इसमें से निकलने का प्रयास करना ही क्यों चाहिये। क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने इसमें से निकलने के तरीके भी तो बता रखे हैं और जो कोई भी वास्तव में इससे निकलना चाहता है उसके लिए सभी साधन जुटा देने का विधान भी बना रखा है। परंतु अधिकांशतः हम इस अयुक्तियुक्त तर्क में फंस कर निरर्थक दलीलें देने लगते हैं कि जब माया भगवान् की ही रची हुई है तो हमें इससे निकलने का प्रयास क्यों करना चाहिये। पर हम भूल जाते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमात्मा से उद्भूत न होती हो। माया से निकलने का सुझाव व तरीके भी तो परमात्मा से ही उद्भूत हैं। इन सबके साथ ही हमें सही-गलत का भेद करने का विवेक भी तो परमात्मा ने ही दे रखा है, इसलिए हमें अपने चयन करने होते हैं। भले सभी कुछ परमात्मा ने ही बनाया है, परंतु उन्हीं परमात्मा ने हमें बुद्धि, विवेक आदि भेद करने की शक्तियाँ भी प्रदान की हैं ताकि उनका उपयोग कर जो सही हो उसका हम वरण कर रहे हैं ऐसी प्रतीति हमें हो सके। यदि हमें ऐसी प्रतीति न हो तो पार्थिव जीवन में चेतना के विकास का वर्तमान ढाँचा कार्य नहीं करेगा। जीवन में सब विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक पाठशाला है जहाँ अनेकानेक प्रलोभन की चीजें हमारे सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं परंतु हमें इन प्रलोभनों से बचते हुए अपने अंतर्निहित स्वभाव के अनुसार सही चीजों का वरण करना होता है। इसे हम लीला कह सकते हैं, आत्मा का विकास कह सकते हैं, यज्ञ का आरोहण कह सकते हैं। अब इसमें यह तर्क देना गलत होगा कि चूंकि प्रलोभन के साधन भगवान् के ही भेजे हुए हैं तो उनमें लिप्त हो जाना सही है। हो सकता है कि वे साधन किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभदायक हों क्योंकि यदि वे निरर्थक ही होते तब तो इस अभिव्यक्ति में उनका अस्तित्व ही नहीं होता। परंतु इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि सभी कुछ ही हमारे लिए उपयोगी है। हमें तो सदा अपने आंतरिक गठन के अनुसार और उसके दृष्टिकोण से चयन करना ही होगा। बहुत से लोगों को हम यह कहते सुनते हैं कि आखिर अमुक काम तो करना अच्छा ही है, या फिर पांडिचेरी स्थित श्रीअरविन्द आश्रम में जाना तो हमेशा अच्छा ही है, या फिर अन्य ऐसी ही कोई चीज करना तो अच्छा ही है। परंतु यदि ये सभी चीजें सभी के लिए सदा ही अच्छी होतीं तो भगवान् स्वयं भी वैसी व्यवस्था कर सकते थे, उनकी ऐसी कोई असमर्थता नहीं है कि वे सभी को वह अच्छी चीज प्रदान नहीं कर सकते थे। परंतु प्रत्येक का गठन भिन्न है और इस कारण उसके लिए चीजों का महत्त्व और उपयोगिता भी बिल्कुल भिन्न होती है। इसलिए किसी एक के लिए अमृततुल्य वस्तु किसी दूसरे के लिए विष समान हो सकती है और जो आज हमारे लिए विषतुल्य है वही अन्य किसी काल में हमारे लिए अमृततुल्य हो सकती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने सदा ही देश-काल-पात्र का मूल मंत्र अपनाया और उसी के आधार पर वे निर्णय किया करते थे। इसलिए भगवान् जहाँ माया के फंदे में फँसाते हैं वहाँ वे उससे निकलने के लिए योग का विधान भी तो देते हैं। इसीलिये तो स्वभाव नियत कर्म की महत्ता है। यदि चयन का विधान न होता तब तो नियत कर्म या फिर अनियत कर्म का तो कोई विकल्प ही नहीं बचता। स्वभाव नियत कर्म का अर्थ यही है कि व्यक्ति सचेतन रूप से उन कर्मों का चयन करता है जो उसके अंदर परम प्रभु की होने वाली विशिष्ट अभिव्यक्ति की ओर ले जाते हैं। हालाँकि अंततः व्यक्ति पहुँचता तो उसी गंतव्य पर है परंतु साधारण जीवन बड़े ही टेढ़े-मेढ़े मार्गों से होकर वहाँ तक जाता है, वहीं श्रीमाताजी कहती हैं कि योग मार्ग सीधे ही गंतव्य तक ले जाता है। भौतिक रूप से तो हम इस बात के बेतुकेपन को समझते हैं कि चूंकि सभी मार्ग भगवान् के ही बनाए हुए हैं इसलिए हमें दाएँ या बाएँ मुड़ने में भेदभाव नहीं करना चाहिये और समान भाव अपनाकर जिस किसी में भी मुड़ जाना चाहिये। कोई स्थूल व्यक्ति भी यह समझता है कि ऐसा करने से तो व्यक्ति कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाएगा, परंतु जब यही बात आध्यात्मिक मार्गों पर लागू की जाती है, जो कि अनंतविध हैं, अनंतस्तरीय हैं तब हम इस तर्क को इस पर लागू करने से चूक जाते हैं।
प्रश्न : भगवान् कहते हैं कि अधियज्ञ का प्रभु मैं स्वयं हूँ। तब अक्षर परमं और अधियज्ञ में अंतर क्या है?
उत्तर : वास्तव में परम सत्ता तो अपने आप में एक ही है और कहीं कोई भेद नहीं है। परंतु उनके भिन्न भावों के निरूपण के लिए भिन्न पदों का प्रयोग होता है। 'अधियज्ञ' से अभिप्रेत है अखिल कर्म और यज्ञ के प्रभु, भगवान् परमेश्वर, पुरुषोत्तम जो यहाँ इन सब देहधारियों के शरीर में गुप्त रूप से विराजमान हैं। यह सारी सृष्टि एक प्रकार का यज्ञ ही है और जिस कारण से यह यज्ञ है और परमात्मा के जिस स्रष्टा भाव को यह चरितार्थ करता है उसे अधियज्ञ कहते हैं। और परमात्मा का वह भाव जो इस सृष्टि क्रम में भाग नहीं लेता, अप्रत्यक्ष रूप से इसे केवल अवलंब प्रदान करता है उसे अक्षर परमं की संज्ञा दी जाती है। मूल रूप से दोनों भाव उसी एक परम सत्ता के ही हैं।
प्रश्न : इस वाक्य का क्या अर्थ है, "जो प्रत्येक जीव का अंतर्निहित सत्य और आत्मतत्त्व है, जो अपने-आप को अभिव्यक्ति में लाता है, जो सबके अंदर निहित वह मूलभूत भागवत् प्रकृति है जो सब प्रकार के परिवर्तनों, विपर्ययों और पुनरावर्तनों के पीछे सदा बनी रहती है, वही स्वभाव है।"
उत्तर : परमात्मा जब कोई व्यक्तित्व धारण कर अपनी कोई एक क्रियाविशेष तथा अपनी एक अभिव्यक्ति विशेष करना चाहते हैं तो उस अभिव्यक्ति का सारा प्रारूप ही स्वभाव है। प्रकृति उस प्रारूप को चरितार्थ करने के लिए आवश्यक साधन जुटाती है। स्वभाव को समझने के लिए हम उसकी तुलना किसी भवन के प्रारूप से, उसकी रूपरेखा से कर सकते हैं। अब उस रूपरेखा के आधार पर इंजीनियर सामान एकत्रित करता है। भले ही बाजार में अनेकों प्रकार की अन्य चीजें भी उपलब्ध हों परंतु वह उन्हीं का चयन करता है जो उस रूपरेखा के अनुकूल हों। उसी प्रकार भगवान् की अभिव्यक्ति की यह रूपरेखा, जो कि स्वभाव है, विश्व-प्रकृति के पास आती है और वह उसे चरितार्थ करने के लिए सभी आवश्यक साधन जुटाने का कार्य करती है। इसीलिए अंतर्निहित स्वभाव ही सबसे प्रभावी चीज है। स्वभाव नियत कर्म इसीलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यों तो असंख्यों प्रकार के कर्म हैं परंतु व्यक्ति किन का चयन करे यह तो उसे उसके स्वभाव से ही पता लग सकता है और उस व्यक्ति के लिए वे ही सच्चे कर्म होते हैं।
यह सब उत्पत्ति तथा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में निरंतर परिवर्तन ही कर्म, प्रकृति का कार्य है, उस प्रकृति की ऊर्जा है जो कर्मकर्ती है और सब क्रिया-प्रणालियों की ईश्वरी है। प्रथमतः यह स्वभाव का अपने को सृष्टिकर्म में डाल देना है, इसी को विसर्ग कहते हैं। यह सृष्टिकर्म भूतों को उत्पन्न करनेवाला, भूतकरः, है और यह सृष्टिकर्म ये भूत आत्मनिष्ठ रूप से अथवा अन्य प्रकार से जो कुछ बनते हैं उसे भी उत्पन्न करनेवाला, भावकरः, है। सब मिलकर, यह काल के अन्दर पदार्थों की सतत् उत्पत्ति या 'उद्भव' है जिसका मूलतत्त्व कर्म की सृजनात्मक ऊर्जा है। यह सारा क्षरभाव अर्थात् 'अधिभूत' प्रकृति की शक्तियों के सम्मिलन से निकल कर आता है, यह अधिभूत ही जगत् है और जीव की चेतना का विषय है। इस सब में जीव ही प्रकृतिस्थ भोक्ता और साक्षीभूत देवता है; बुद्धि, मन और इंद्रियों की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जीव की चेतन सत्ता की जो समस्त शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा यह प्रकृति की इस क्रिया को प्रतिबिंबित करता है, इसके 'अधिदैव' अर्थात् अधिष्ठातृदेवता हैं। यह प्रकृतिस्थ जीव ही इस तरह क्षर पुरुष है, भगवान् का नित्य कर्म-स्वरूप हैः यही जीव प्रकृति से ब्रह्म में लौटकर अक्षर पुरुष, भगवान् का नित्य नैष्कर्म्य-स्वरूप, होता है। परंतु क्षर पुरुष के रूप और शरीर में परम् पुरुष भगवान् ही निवास करते हैं। अक्षरभाव की अचल शान्ति और क्षरभाव के कर्म का आनन्द दोनों ही भाव एक साथ अपने अन्दर रखते हुए भगवान् पुरुषोत्तम मनुष्य के अन्दर निवास करते हैं। वे हमसे दूर परे किसी परम् पद पर ही स्थित नहीं हैं, अपितु वे यहाँ प्रत्येक प्राणी के शरीर में, मनुष्य के हृदय में और प्रकृति में भी विद्यमान हैं जहाँ वे प्रकृति के कर्मों को यज्ञरूप से ग्रहण करते हैं और मानव जीव के सचेतन आत्म-दान की प्रतीक्षा करते हैंः परन्तु हर हालत में, मनुष्य की अज्ञानावस्था और अहंकारिता में भी वे ही उसके स्वभाव के स्वामी और उसके सब कर्मों के प्रभु होते हैं, जो प्रकृति और कर्म विधान पर अधिष्ठातृत्व करते हैं। उन्हीं से निकलकर जीव प्रकृति की इस क्षर-क्रीड़ा में आता है और अक्षर आत्मसत्ता से होता हुआ उन्हीं के परम धाम को प्रास होता है।
इस संक्षिप्त विवरण के तुरंत बाद गीता ज्ञान द्वारा परम मोक्ष के विचार के विवेचन की ओर अग्रसर होती है जिसका निर्देश पूर्वाध्याय के अन्तिम श्लोक में गीता ने किया है।
इस प्रकार गीता में हम विश्व के निर्माण के अनेक तरीके के वर्णन पाते हैं। वेदों में भी हम इसका एक भिन्न वर्णन पाते हैं। वेदों में वर्णन मिलता है कि शब्द से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। परंतु यह सारा विषय बिना अनुभव के समझ में नहीं आ सकता। व्यक्ति को इसका जितना ही अधिक अनुभव होगा उतनी ही अच्छी तरह वह इसे समझ सकेगा। आखिर, इस सारी सृष्टि के विषय में हम सचेतन कैसे होते हैं? हमारी इंद्रियाँ अपनी सूचना मनस् के पास भेजती हैं जहाँ सारा प्रतिबिंब बनता है। मनस् इस सारी सूचना के साथ अपने स्वयं के बोधों को जोड़कर बुद्धि के पास भेजता है। वहाँ सारा दृश्य तैयार होता है और वहीं से क्रिया-प्रतिक्रिया का निर्णय आता है। इसलिए हमारे अंदर जो मनोवैज्ञानिक तथा आत्मपरक शक्तियाँ हैं उन्हीं के प्रभाव से हमें यह सृष्टि ऐसी प्रतीत होती है। इन्हीं शक्तियों को अधिदैव कहते हैं। वास्तव में अपने आप में ऐसी कोई सृष्टि है ही नहीं। स्वयं सांख्यशास्त्र भी इसका वर्णन करते हुए हमें यह दर्शाता है कि हमारे गठन के कारण ही हमें इस प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है। अपने आप में इसका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है। इसी सृष्टि को भिन्न-भिन्न जीव भिन्न-भिन्न रूप में देखते हैं। वहीं यदि किसी जीव का गठन सर्वथा भिन्न प्रकार का होगा तो उसे तो इस सृष्टि का भान एकदम भिन्न प्रकार से होगा और इसी कारण उसकी चेतना के लिए वे नियम बाध्यकारी नहीं होंगे जो हमारे लिए होते हैं। इसलिए जैसा प्रारूप प्रभु ने हमारे अंदर निहित कर रखा है वैसा ही हमें अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों की सहायता से प्रतीत होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जगत् में अकेले ही निवास करता है, उसमें कोई दूसरा नहीं रहता। अवश्य ही व्यक्ति एक ऐसी चेतना में भी प्रवेश कर सकता है जहाँ उसे यह अनुभव हो कि सभी शरीरों में स्वयं वही विद्यमान है। जब तक हम इंद्रियों आदि के द्वारा बँधे होते हैं तब तक हमें दृश्य जगत् की भौतिक यथार्थता पर बहुत अधिक आग्रह रहता है। परंतु जैसे-जैसे व्यक्ति अपनी गहराइयों में प्रवेश करने लगता है, वैसे-वैसे उसका यह भ्रम टूटता जाता है। इसीलिए चमत्कार संभव हैं क्योंकि वास्तव में तो सारी संरचना ही मनोवैज्ञानिक है। ऐसी कोई भौतिक चीज तो कुछ है ही नहीं जो कि नमनीय न हो। इसलिए सारी मनोवैज्ञानिक संरचना भगवान् के उस विशिष्ट भाव के अनुसार होती है जो वे प्रत्येक जीवविशेष के अंदर भिन्न-भिन्न रूप से प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण जीव के लिए सच्ची समझदारी तो इसी में है कि वह उस विशिष्ट भाव के प्रति सचेतन हो और अधिकाधिक उसी के अनुरूप कार्य करे। इसी को चेतना का विकास कहते हैं जिसमें व्यक्ति अधिकाधिक भीतर के उस भाव के संपर्क में आता जाता है और उसी के द्वारा अपने समस्त क्रियाकलाप को निर्धारित करता है। इस रहस्य को भली-भाँति जानने के कारण ही भारतीय संस्कृति का सारा ध्यान इसी पर था कि किस प्रकार यथाशीघ्र प्रत्येक जीव को उसके उस अंतर्निहित भाव के संपर्क में लाया जाए क्योंकि एक बार उसके संपर्क में आने पर स्वतः ही वह उसके अनुसार अपने सारे क्रियाकलाप स्वभाव नियत रूप से करने लगेगा और तब किसी भी प्रकार के बाहरी विधान की आवश्यकता मंद होती जाएगी व अन्त में - जब पूर्ण रूपांतर साधित हो जाएगा तब - आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
सारा खेल ही चेतना का है। जब सारा दृश्य भीतर से प्रक्षिप्त हो रहा है तब बाहरी दृश्य से विचलित होने की मूलतः तो कोई आवश्यकता हो नहीं है। और चूँकि सब कुछ भीतर ही है तो केवल बाहरी अन्वेषण-विश्लेषण से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए श्रीअरविन्द ने कहा कि, "अतिचेतन ही वस्तुओं का सच्चा आधार है, न कि अवचेतन। कमल का यथार्थ महत्त्व उस कीचड़ के रहस्यों का विश्लेषण करने से नहीं मिलेगा जिसमें से वह यहाँ उगता है; उसका रहस्य तो कमल के उस दिव्य आदिरूप में मिलेगा जो नित्य ही ऊपर प्रकाश में कुसुमित होता है।"* अब जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तब जाकर हमें समझ में आता है कि सत्य को खोजने का विज्ञान का तरीका तो सर्वथा उल्टा है। चीजों को सच्चे रूप में केवल चेतना के द्वारा ही समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए भले हम अपने किसी पालतू पशु को पूरे अमरीका की सैर करा लाएँ फिर भी वह वहाँ का क्या वर्णन कर सकता है? वहीं, कोई समझदार व्यक्ति वहाँ की एक झलक मात्र पाने के बाद भी हमें वहाँ की कुछ सूचना अवश्य दे सकता है। इस चीज को समझे बिना यदि कोई केवल जड़ भौतिक तत्त्व के आधार पर सत्य तक पहुँचने का प्रयास करे तो यह सर्वथा निरर्थक होगा। इस संदर्भ में विज्ञान के विषय में श्रीअरविन्द की यह उक्ति अत्यंत प्रकाशक है, "यदि तुम भागवत् यथार्थता या सद्वस्तु को चूक जाओ या उसकी उपेक्षा कर दो तो चीजों का कोई मूलभूत सार नहीं रह जाता; क्योंकि तुम कामचलाऊ और उपयोग करने योग्य ऊपरी दिखावे की अतिविशाल सतही परत में धँसे रहते हो। तुम दिव्य जादूगर के जादू का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हो, परंतु जब तुम स्वयं जादूगर की चेतना में प्रवेश करते हो केवल तभी तुम लीला के सच्चे उद्गम, उसके अर्थ और उसके घेरों का अनुभव करना शुरू करते हो। मैं कहता हूँ 'शुरू करते हो' क्योंकि दिव्य सद्वस्तु इतनी सरल नहीं है कि पहले ही स्पर्श में तुम उसका सब कुछ जान लो या उसे किसी एक ही सूत्र में डाल दो; यह तो स्वयं अनंत है और तुम्हारे समक्ष एक अनंत ज्ञान को खोलता है जिसके आगे सारा विज्ञान कुल मिलाकर भी एक तुच्छ-सी वस्तु है।" (CWSA 28, 332) इसलिए सच्चा सार इसी में है कि व्यक्ति अपने भीतर जाए, चेतना का विकास करे, अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करे और उसी को अभिव्यक्त करे। केवल ऐसा करने से ही व्यक्ति को सच्चा सुख, सच्ची परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है अन्यथा निजस्वरूप से भिन्न रूप में जीने से तो किसी भी प्रकार की सच्ची परिपूर्णता कभी मिल ही नहीं सकती। इसीलिए श्रीअरविन्द कहते हैं, "दिव्य जीवन की ओर आरोहण ही मानव यात्रा है, कर्मों का 'कर्म' और स्वीकार करने योग्य 'यज्ञ' है। यही जगत् में मनुष्य का एकमात्र वास्तविक कार्य तथा उसके अस्तित्व का औचित्य है, जिसके बिना वह भौतिक ब्रह्माण्ड की भयंकर विशालताओं के बीच सतही कीचड़ व पानी के संयोग से अपने-आप बने एक छोटे-से कण - पृथ्वी - पर अन्य क्षणभंगुर कीटों के बीच एक रेंगता हुआ कीट मात्र ही रहेगा।" (CWSA 21, 48)
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।। ५।।
५. और जो मनुष्य अपने जीवन के अंत समय में केवल मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ कर प्रयाण करता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है; इसमें कोई संशय नहीं है।
यं यं वापि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।। ६।।
६. हे कौन्तेय! जो कोई मनुष्य अन्त समय में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह उस ही भाव को प्राप्त होता है जिस भाव में वह जीव अपने भौतिक जीवनकाल में निरंतर आंतरिक रूप से बढ़ रहा था।
मनुष्य संसार में जन्म लेकर प्रकृति और कर्म की क्रिया में लोक-परलोक के चक्कर काटता रहता है। प्रकृति में स्थित पुरुष - यही उसका सूत्र होता है: उसके अंदर उसकी आत्मा जो कुछ सोचती, मनन करती और कर्म करती है, वह सदा वही बन जाता है। वह जो कुछ पहले रहा है उसी ने उसके वर्तमान जन्म को निर्धारित किया है; और जो कुछ वह है, जो कुछ वह सोचता और इस जीवन में अपनी मृत्यु के क्षण तक करता रहता है वही निश्चित करता है कि वह मृत्यु के बाद परलोकों में और अपने भावी जीवनों में क्या बनेगा। जन्म यदि 'होना' है तो मृत्यु भी एक 'होना' ही है, किसी भी प्रकार यह समाप्ति नहीं है। शरीर छूट जाता है, परंतु जीव, 'त्यक्त्वा कलेवरम्' शरीर को छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। अतः बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि अपने प्रयाण के संधि-क्षण में वह क्या होता है। क्योंकि मृत्यु के समय संभूति के जिस भी रूप पर उसकी चेतना स्थिर होती है और मृत्यु के पूर्व जिसमें उसकी मन-बुद्धि सदा तन्मय रहती आयी है उसी रूप को वह अवश्य प्राप्त होता है; क्योंकि प्रकृति कर्म के द्वारा जीव के सब विचारों और वृत्तियों को ही कार्यान्वित किया करती है और वास्तव में यही प्रकृति का सारा कार्य-व्यापार है। इसलिए मनुष्य में स्थित जीव यदि पुरुषोत्तम-पद लाभ करना चाहता है तो उसके लिए दो आवश्यकताएँ हैं, वह संभव हो सके उससे पूर्व दो शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है। एक यह कि इस पार्थिव जीवन में रहते हुए उसने अपना संपूर्ण आंतरिक जीवन उसी आदर्श की दिशा में गढ़ा हो; और दूसरी यह कि प्रयाण-काल में उसकी अभीप्सा और संकल्प उस आदर्श के प्रति सच्चे बने रहें।
-----------------------------------
Sri Aurobindo to Dilip, Vol.1, 2003, p.189, Hari Krishna Mandir Trust. Pune, and Mira Aditi, Mysore
प्रश्न : इसमें बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना जिस भी चीज पर स्थिर होती है वह उसी रूप को प्राप्त होता है। तब फिर व्यक्ति के पूरे जीवन-काल में उसने जो कुछ भी क्रिया-कलाप किया, क्या उसका कोई महत्त्व नहीं?
उत्तर : सामान्यतः तो व्यक्ति अपने पूरे जीवन-काल में जो भी सोचता या जिस भी चेतना में रहता है, अंतिम समय में भी उसकी चेतना उन्हीं चीजों में फँसी रहती है। परन्तु ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन-काल में जो सोचता या जिस चेतना में रहता है, उससे भिन्न या विपरीत कोई चीज उसके अंतिम क्षणों में आ जाए, और ऐसे में वही प्रभावी होगी। उदाहरण के लिए अजामिल, जिसने कि अपने जीवन-काल में कोई सत्कर्म नहीं किया था और न ही वह कभी भगवान् का स्मरण ही करता था, परन्तु अपने अंतिम क्षणों में उसने अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा। ऐसा उसने एकाग्र होकर भगवान् को स्मरण कर के नहीं किया क्योंकि उसे तो भगवान् से कोई सरोकार नहीं था, उसने तो मोहवश अपने पुत्र का नाम पुकारा था। परन्तु फिर भी भगवान् के पार्षद उसे लेने आए और उसे सद्गति की प्राप्ति हई। विरले ही लोगों के अंतिम क्षणों में भगवान् का नाम उनके मुख पर आता है।
प्रश्न : यदि अंत समय में किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्या गति होती है?
उत्तर : सामान्यतः तो ऐसे व्यक्तियों की कोई अच्छी गति नहीं होती, हालाँकि व्यक्ति की अंतरात्मा का, उसके चैत्य पुरुष का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ जिस बारे में बताया जा रहा है वह सब तो प्राणिक सत्ता के साथ होता है। जब अंतरात्मा ने एक बार मनुष्य शरीर धारण कर लिया है तब वह उस अवस्था से नीचे नहीं गिर सकती और न ही उसकी कभी कोई दुर्दशा हो सकती है क्योंकि वह तो भगवान् का अंश है, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य जहाँ होता है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश फैलता है, अंधकार उसे नहीं दबा सकता, उसी प्रकार अंतरात्मा का भी कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता।
प्रश्न : अंत समय में यदि कोई बीमारी से ग्रस्त हो तो वह तो अपनी बीमारी में ही त्रस्त रहेगा, उसी पर केन्द्रित रहेगा। उसे तो भगवान् का स्मरण हो ही कैसे सकता है?
उत्तर : इसीलिए तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन-काल में साधना नहीं करता और परमात्मा को याद नहीं करता तो अंतिम क्षणों में उसको परमात्मा की याद बनी रहना लगभग असंभव है। फिर भी यदि किसी कारण से या संयोगवश परमात्मा की याद आ जाए - जिसकी कि संभावना बहुत कम होती है - तो वह बहुत कारगर होती है। परन्तु यदि जीवनपर्यंत व्यक्ति साधना करता है तो अंतिम क्षणों में भगवान् का स्मरण होना एक निश्चिति हो जाती है।
प्रश्न : क्या प्राण छूटते ही आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है?
उत्तर : श्रीमाताजी के अनुसार सामान्य तौर पर चैत्य पुरुष जितना ही अधिक विकसित होता है उतना ही अधिक समय वह दूसरा जन्म ग्रहण करने में लेता है क्योंकि शरीर में रहते समय चैत्य जितने ही अधिक अनुभव ग्रहण करता है उसके बाद उतना ही समय उसे उन्हें आत्मसात् करने में लगता है। यदि चैत्य पुरुष अभी अधिक विकसित नहीं है तव तो शरीर त्याग के बाद उसका पुनर्जन्म जल्दी ही हो जाता है। श्रीमाताजी के अनुसार ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ मृत्यु के बाद वह उसी परिवार में पुनः जन्म ग्रहण कर लेता है। परंतु यह क्षेत्र या यह विषय इतना विस्तृत है कि किन्हीं सीधे-सादे नियमों में इसे नहीं बाँधा जा सकता।
मनुष्य जब से पैदा होता है तब से उसके मन, प्राण और शरीर की दीवारें आत्मा के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं इसलिए व्यक्ति के सचेतन होते ही जीवन का एक ही उद्देश्य रह जाता है और वह है उन दीवारों को तोड़ना। परन्तु हमारे बाहरी भागों को इसमें कोई रुचि नहीं होती कि वे दीवारें टूटें क्योंकि इनके पीछे जो तामसिक शक्तियाँ कार्य करती हैं वे कभी नहीं चाहतीं कि कोई प्रकाश आ जाए और अंधकार में चलती उनकी क्रियाकलाप में कोई व्यवधान पड़े, इसलिए वे इसका विरोध करती हैं। अब जैसे किसी नाबालिग राजा के मंत्री जो अपनी मनमानी करते हैं वे कभी नहीं चाहेंगे कि वह राजा बालिग हो और उन पर अंकुश लगाए और शासन करे, वैसे ही ये शक्तियाँ भी नहीं चाहतीं कि आत्मा को धरती पर अभिव्यक्त होने का मौका मिले अन्यथा उनका निरंकुश खेल तो खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए साधना इतनी कठिन होती है। परन्तु इसका लाभ यह है कि व्यक्ति इन शक्तियों के खेल को धीरे-धीरे समझ जाता है और तब वह अधिकाधिक आत्मा की शक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान कर इन शक्तियों के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करना सीख जाता है और अंततोगत्वा अन्धकार की शक्तियों व उनके क्रियाकलाप के पीछे भी जो भागवत् सत्य छिपा हुआ है उसे आत्मसात् कर पाता है।
गीता इस प्रसंग में मृत्यु के समय के विचार और मनःस्थिति पर बड़ा महत्त्व देती है, एक ऐसा महत्त्व जिसे समझना हमारे लिए बहुत कठिन होगा यदि हम उस चीज को न स्वीकार करते हों जिसे चेतना की आत्म-सृजनात्मक शक्ति कहा जा सकता है। हमारा विचार, हमारी आंतरिक दृष्टि, हमारी श्रद्धा जिस बात पर पूर्ण और सुनिश्चित बल के साथ अपने-आप को सुस्थिर करती है, उसी (के स्वरूप) में हमारी आंतरिक सत्ता परिवर्तित होने लगती है। यह प्रवृत्ति तब एक निर्णायक शक्ति बन जाती है जब हम उन उच्चतर आध्यात्मिक और आत्म-विकसित अनुभवों को प्राप्त होते हैं जो बाह्य पदार्थों पर उतने निर्भर नहीं होते जितनी कि बाह्य प्रकृति के वशीभूत होने के कारण हमारी सामान्य मनोवृत्ति हुआ करती है। वहाँ हम अपने-आप को स्थिरतापूर्वक वह बनते हुए देख सकते हैं जिस पर हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और जिसकी हम निरंतर अभीप्सा करते हैं। इसलिए वहाँ अपने विचार का थोड़ी देर के लिए भी छूट जाना, स्मरण में जरा-सी भी अशुद्धता के आ जाने का अर्थ है इस परिवर्तन की प्रक्रिया में एक गतिरोध या फिर इस परिवर्तन-क्रिया से पतन और हम जो पहले थे उसी की ओर पीछे लौटना, ऐसी आशंका तब तक रहती है जब तक कि कम-से-कम हमने अपने नवीन भाव को काफी हद तक और अटल रूप से स्थापित अथवा सुदृढ़ न कर लिया हो। जब हमने यह कर लिया हो, जब हमने उसे सामान्य अनुभव बना लिया हो तब उसकी स्मृति स्वतःविद्यमान रूप से रहती है, क्योंकि अब वह हमारी चेतना का ही स्वाभाविक रूप होती है। मर्त्य जगत् से प्रयाण करने के संधि-क्षण में हमारी चेतना की तात्कालिक स्थिति का महत्त्व इससे स्पष्ट हो जाता है। परंतु यह कोई मरण-शय्या पर किया गया स्मरण नहीं है जो हमारी संपूर्ण जीवनधारा से और हमारी पूर्व मनःस्थिति से बेमेल हो या फिर जिसकी इनके द्वारा अधूरी तैयारी हुई हो। ऐसे स्मरण के अंदर कोई उद्धारक शक्ति नहीं हो सकती। यहाँ गीता का जो विचार है वह प्रचलित धर्म की रियायतों और सुविधाओं के ही समान नहीं है; इसका इन सनकों से कोई सरोकार नहीं है कि एक पूरा अपवित्र सांसारिक जीवन बिताने के बाद पादरी के द्वारा अंत में सर्वप्रायश्चित करा लेने से ही ईसाई मरण-काल में पावन हो जाता है अथवा पहले से ही ध्यान रखकर या अकस्मात् पवित्र काशीधाम में या पवित्र गंगा के तट पर मर जाने से और अंत में पंडित द्वारा अंतिम-क्रियाएँ कराने से मुक्ति मिल जाती है, गीता के अनुसार यह मोक्ष की कोई पर्याप्त प्रणाली नहीं है। जिस दिव्य भाव पर मन को प्रयाणकाल में अचल रूप से स्थिर करना होता है, 'यं स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम्', वह तो वही भाव होना चाहिए जिसकी ओर जीव अपने सांसारिक जीवन में प्रतिक्षण आगे बढ़ता रहा हो, सदातद्भावभावितः।
अंत समय के स्मरण का ही एक उदाहरण देते हुए श्रीमाताजी ने बताया कि श्रीअरविन्द आश्रम के ही एक साधक ने कुछ धार्मिक पुस्तकें आदि पढ़ रखी थीं और उसमें आए स्वर्गों आदि के वर्णन से वह प्रभावित था। इसलिए मृत्यु के उपरान्त वह ऐसे ही किसी एक मनोनिर्मित स्वर्ग में पहुँच गया। चूंकि श्रीमाताजी तो जानती थीं कि ऐसे स्वर्ग आदि की केवल सापेक्ष वास्तविकता ही होती है इसलिए वे उसे उसमें से निकाल कर किसी सत्यतर जगत् में ले जाना चाह रही थीं। परंतु वह व्यक्ति उस स्वर्ग की चकाचौंध से इतना प्रभावित था कि श्रीमाताजी को उसे उस जगत् की सापेक्षता समझाकर वहाँ से निकालने में लगभग एक वर्ष का समय लग गया। जब श्रीमाताजी इस उदाहरण का उल्लेख कर रही थीं तो किसी ने पूछा कि आखिर ये जगत् कितने वास्तविक हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया कि ये जगत् अधिक वास्तविक तो नहीं हैं परंतु वर्तमान में हम जिस जगत् में निवास कर रहे हैं, जिसमें हमें इंद्रियों आदि के माध्यम से स्पर्श-बोध आदि प्राप्त होते हैं और जिसे हम बिल्कुल वास्तविक मानते हैं, उससे ये कुछ अधिक वास्तविक हैं। अब इस कथन से हमें अपने वर्तमान जगत् की घोर अवास्तविकता का और इसकी सापेक्षता का भान होता है जिसे कि वास्तविक मानकर हम पूरे जीवन इससे अभिभूत रहते हैं और जीवन में कभी किसी गहरे और सार्थक उद्देश्य के विषय में सोचते तक नहीं।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ।। ७।।
७. इसलिए सभी समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर; क्योंकि यदि तेरा मन और तेरी बुद्धि सदा मुझमें स्थिर और मेरे प्रति अर्पित होगी, तो निःसंदेह ही तू मुझे प्राप्त होगा।
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ।। ८।।
८. हे पार्थ! निरन्तर अभ्यासरूप योग के द्वारा, भगवान् के साथ युक्त हुई और अन्यत्र कहीं विचलित न होनेवाली चेतना से, सर्वदा भगवान् का चिन्तन करता हुआ मनुष्य दिव्य और परम् पुरुष को प्राप्त होता है।
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।। ९।।
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।
ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।। १० ।।
९-१०. ये परम् पुरुष द्रष्टा (कवि), पुरातन, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, समस्त भूतों के प्रभु और शासक तथा पालक हैं; उनका रूप अचिंत्य है। तम अथवा अंधकार से परे, वे सूर्य के समान ज्योतिर्मय हैं। जो प्रयाण के समय अचल मन से, योग बल से संपन्न और भक्तियुक्त' होता है, जिसने प्राण-शक्ति को पूरी तरह से ले जाकर ध्रुवों के बीच में स्थिर कर दिया है, वह इस परम् पुरुष को प्राप्त होता है।
यहाँ हम इन परम् पुरुष भगवान् के सर्वप्रथम वर्णन पर पहुँचते हैं, - उन परम देव के वर्णन पर पहुँचते हैं जो अक्षर ब्रह्म से भी उत्तम और महान् हैं और जिन्हें गीता आगे चलकर पुरुषोत्तम की संज्ञा देती है। ये भगवान् भी अपनी कालातीत शाश्वत सत्ता में अक्षर हैं और इस समस्त अभिव्यक्ति से अत्यंत परे हैं और यहाँ काल के अन्दर हमें उन 'अव्यक्त अक्षर' की सत्ता की केवल अस्पष्ट झलकियाँ उनके विविध प्रतीकों और छद्मवेशों के द्वारा प्राप्त होती हैं। फिर भी वे केवल निर्गुण-निराकार अथवा अलक्षण, 'अनिर्देश्यम्' ही नहीं हैं; या यह कहिये कि वे अनिर्देश्य केवल इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य की बुद्धि को जिस अत्यंत सूक्ष्मातिसूक्ष्म का बोध है वे उससे भी अधिक सूक्ष्म हैं और इसलिए भी कि भगवान् का स्वरूप अचिंत्य है...
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।। ११ ।।
११. जिसे वेद के जाननेवाले अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जिसमें तपस्वी तब प्रवेश करते हैं जब वे (काम-क्रोधादि) आवेगों से परे जा चुके होते हैं और जिसे प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस पद या स्थिति को मैं तुझे संक्षेप में कहूँगा।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ।। १२।।
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ।। १३ ।।
१२-१३. इन्द्रियों के समस्त द्वारों को संयत करके, मन को हृदय में निरुद्ध करके, अपनी प्राण-शक्ति को मूर्धा (सिर) में ले जाकर स्थिर करके, जो व्यक्ति योग के द्वारा चित्त की एकाग्रता में स्थित हो, एकाक्षर पवित्र शब्द ॐ का उच्चारण करता है, और प्रयाणकाल में मुझे स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है।
[यही] प्रयाण की प्रचलित यौगिक पद्धति है, संपूर्ण सत्ता को शाश्वत, परात्पर के प्रति अंतिम रूप से भेंट करना। परंतु फिर भी यह केवल एक पद्धति है; मूलभूत स्थिति है जीवन में, कर्म और युद्ध तक में – मामनुस्मर युद्धय च - भगवान् का सतत् अचल स्मरण करना और संपूर्ण जीवन को निरंतर योग अर्थात् 'नित्ययोग' बना देना। जो कोई भी ऐसा करता है, भगवान कहते हैं कि, वह मुझे अनायास पा लेता है; वही महात्मा है जो परम सिद्धि या पूर्णता लाभ करता है।
----------------------------
...यहाँ ज्ञान के द्वारा निर्गुण निराकार ऐक्य ने प्रेम-भक्ति के द्वारा भगवान् से ऐक्य का स्थान नहीं ले लिया है, अपितु यह भक्तियोग अंत तक परम योगशक्ति का एक अंग बना रहता है…
viii.7
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४।।
१४. हे पार्थ! जो योगी अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ, अनवरत और सतत् रूप से मेरा स्मरण करता है, वह मुझसे नित्य युक्त रहता है और मुझे सुलभता से प्राप्त कर लेता है।
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।। १५।।
१५. मेरे पास आने के बाद, ये महात्मा पुनर्जन्म को, मर्त्य प्राणी की इस अनित्य और दुःखमय स्थिति को, पुनः प्राप्त नहीं करते; वे परम गति को प्रास होते हैं।
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।। १६ ।।
१६. हे कौन्तेया जगत् परंपरा में ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं उन सबसे पुनरावृत्ति (अर्थात् पुनः जन्मग्रहण की क्रिया) होती है, किन्तु उस जीव पर पुनर्जन्म बाध्य नहीं होता जो मुझे प्राप्त कर लेता है।
इस प्रकार ऐहिक जीवन से प्रयाण करके जीव जिस स्थिति में पहुँचता है वह विश्वातीत स्थिति है। इस लोकपरंपरा के अन्दर जो उत्तमोत्तम स्वर्गलोक हैं वे सब पुनरावृत्ति के अधीन हैं; परंतु जो जीव पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है उस पर पुनर्जन्म बाध्य नहीं होता। अतः अनिर्देश्य ब्रह्म को प्राप्त करने की ज्ञानाभीप्सा से जो कुछ फल प्राप्त हो सकता है वही इन स्वतःसिद्ध परम् पुरुष को, जो सब कर्मों के अधीश्वर तथा सब मनुष्यों और प्राणियों के सुहृद् हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति (प्रेम) के द्वारा प्राप्त होने की अभीप्सा के इस दूसरे और व्यापक मार्ग से भी प्राप्त होता है। उन भगवान् को इस प्रकार जानना और इस प्रकार उनकी खोज करना पुनर्जन्म से या कर्म-श्रृंखला से नहीं बाँधता; जीव इस मर्त्य जीवन की क्षणभंगुर और क्लेशदायिनी स्थिति से सदा के लिए मुक्त होने की अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। और, गीता इस जन्मचक्र तथा इससे छूटने की बात को बुद्धि के लिए और भी अधिक सटीक बनाने के लिए विश्व के (सृष्टि और लय संबंधी) चक्रों के उस प्राचीन सिद्धांत को स्वीकार कर लेती है, जो कि विश्वप्रपंचसंबंधी भारतीय धारणाओं का एक स्थायी अंग बन गया था।
v.29
सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः ।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। १७।।
१७. जो लोग, ब्रह्मा का एक दिन जो कि एक सहस्र युगी तक रहता है, और रात्रि जो एक सहस्र युगांत तक रहती है, ऐसा जानते हैं, वे दिन और रात को जाननेवाले हैं।
अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥
१८. ब्रह्मा के दिन के आने पर अव्यक्त में से समस्त चराचर उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आने पर सभी उस अव्यक्त में लय हो जाते हैं।
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । रा
त्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ।। १९।।
१९. हे पार्थ! यह समस्त चराचर भूतों का समूह असहाय रूप से बार-बार अभिव्यक्ति में आता है, रात्रि आने पर लय हो जाता है और दिन आने पर उत्पन्न हो जाता है।
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २०॥
२०. किन्तु इस (वैश्विक) अव्यक्त से परे, सत्ता का एक दूसरा विश्वातीत अव्यक्त सनातन स्वरूप है, जो समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है।
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।। २१ ।।
२१. वह 'अव्यक्त अक्षर' कहा जाता है, उसे परम-आत्मा, परम-पद कहते हैं, जो उसे प्रास कर लेते हैं वे लौटकर नहीं आते; वह मेरा परम धाम है।
चाहे हम विश्व की उत्पत्ति-प्रलय संबंधी इस धारणा को ग्रहण करें या रद्द कर दें, - क्योंकि यह इस पर निर्भर है कि हम 'दिन और रात के जाननेवालों' के ज्ञान को कितना महत्त्व प्रदान करते हैं, पर महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि गीता इसे क्या मोड़ देती है। सहज ही कोई समझ सकता है कि यह शाश्वत रूप से अव्यक्त सत्ता, जिसका इस व्यक्त-अव्यक्त जगत् के साथ कुछ भी संबंध नहीं प्रतीत होता, वह अवश्य ही नित्य अलक्षित अनिर्वचनीय निरपेक्ष सत्ता होनी चाहिये, और उस तक पहुँचने का उचित मार्ग होगा कि जो कुछ हम अभिव्यक्ति में बन गए हैं उस सबसे छुटकारा पा लें, यह नहीं कि अपनी बुद्धि के ज्ञान को, हृदय की प्रेम-भक्ति को, योगसंकल्प को और प्राण की प्राणशक्ति को एक साथ एकाग्र करके संपूर्ण अंतश्चेतना को उसकी ओर ले जाएँ। विशेषतः, भक्ति तो उस परम निरपेक्ष के संबंध में अनुपयुक्त ही प्रतीत होती है जो कि सभी संबंधों से रिक्त है, 'अव्यवहार्य' है। 'परन्तु' गीता आग्रहपूर्वक कहती है कि यद्यपि यह स्थिति विश्वातीत और यह सत्ता सदा अव्यक्त है, तथापि 'उन परम् पुरुष को... भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करना होता है।...'
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ।। २२ ।।
२२. हे पार्थी परन्तु उस परम् पुरुष को, जिसके भीतर समस्त भूत रहते हैं, जिससे यह सम्पूर्ण जगत् विस्तृत हुआ है, अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है।
vii. 19
दूसरे शब्दों में कहें तो, वे परम् पुरुष हमारी मिथ्या-माया से उदासीन सर्वथा संबंधरहित र निरपेक्ष नहीं हैं, अपितु जगतों के द्रष्टा (कवि), स्रष्टा और शासक हैं, 'कविं, अनुशासितारं, धातारं', और उन्हीं को 'एक' और 'सर्व', वासुदेवः सर्वमिति, के रूप में जानकर और उन्हीं की भक्ति करके हमें अपनी संपूर्ण सचेतन सत्ता से सब पदार्थों, सब शक्तियों, सब कर्मों में उनके साथ ऐक्य के द्वारा परम चरितार्थता, पूर्ण सिद्धि, परम मुक्ति खोजनी चाहिए।
--------------------------------------
* यदि परम् पुरुष हमारे साथ सम्बन्ध रखने में समर्थ भी होते, पर केवल निर्वैयक्तिक सम्बन्ध ही, तो धर्म मानव प्राणसत्ता के लिए अपना महत्त्व खो बैठता और भक्तिमार्ग भी फलदायक या यहाँ तक कि सम्भव ही नहीं रहता। अवश्य ही हम उसके प्रति अपने मानवीय भावों का प्रयोग कर सकते हैं, पर अनिश्चित एवं अयथार्थ ढंग से तथा किसी मानवोचित उत्तर की आशा के बिना : केवल जिस तरीके से वह हमें उत्तर दे सकता है, वह है हमारे संवेदनों को निःस्तब्ध करके और हमें अपनी निर्वैयक्तिक शान्ति एवं निर्विकार समता से आच्छादित करके; और ऐसा ही वस्तुतः होता है जब हम ईश्वर की शुद्ध निर्वैयक्तिकता के पास जाते हैं। हम एक दैवी विधान के रूप में उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, उसकी शान्त सत्ता के प्रति अभीप्सा में अपनी आत्माओं को उसकी ओर ऊपर उठा सकते हैं, अपनी भावुक प्रकृति को अपने से दूर कर के उस निर्वैयक्तिकता में विकसित हो सकते हैं; हमारे अन्दर का मानव-जीव तृप्त तो नहीं होता पर वह शान्त, संतुलित और स्थिर हो जाता है। परन्तु भक्तियोग, जो इस विषय में धर्म से एकमत है, इस निर्वैयक्तिक अभीप्सा की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ एवं स्नेहसिक्त पूजा का आग्रह करता है। यह हमारे अंदर की मानवता की तथा हमारी सत्ता के निर्वैयक्तिक भाग की एक ही साथ दिव्य परिपूर्ति का लक्ष्य रखता है; यह मनुष्य की भावमय प्रकृति की दिव्य परितृप्ति का लक्ष्य रखता है। परम देव से यह हमारे प्रेम को स्वीकार करने की और उसके अनुरूप उत्तर की माँग करता है; जैसे हम उनमें आनन्द लेते तथा उन्हें खोजते हैं वैसे ही, इसका विश्वास है कि, वे भी हममें आनन्द लेते और हमें खोजते हैं! और न ही इस माँग को बुद्धिविरुद्ध कहकर इसकी निन्दा ही की जा सकती है, क्योंकि यदि परम और विश्वमय पुरुष हममें किसी प्रकार का रस न लेते तो यह समझना कठिन है कि हमारा उद्भव सम्भव ही कैसे होता या हम अस्तित्वमान कैसे रह सकते थे, और यदि वे हमें अपनी ओर बिल्कुल भी खींचते नहीं, - यदि भगवान् हमें खोजते ही नहीं, तो प्रकृति में कोई भी ऐसा कारण नहीं दिखता कि क्यों हम उसे खोजने के लिये अपनी सामान्य सत्ता के चक्र से मुँह फेरकर उसकी ओर मुड़ें।
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ।। २३ ।।
२३. और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन ! जिस समय में देह त्याग कर प्रयाण करने पर योगी इस पृथ्वी लोक में फिर जन्म न ग्रहण करने और फिर जन्म ग्रहण करने-रूप गति को प्राप्त करते हैं उस काल को मैं तुम्हें बतलाता हूँ।
[यहाँ] एक अधिक अनोखी बात आती है जिसे गीता ने प्राचीन वेदान्त के रहस्यवादियों से ग्रहण किया है। यहाँ यह उन भिन्न-भिन्न कालों का निर्देश करती है जिन कालों में योगी को अपनी इच्छानुसार, यह चुनाव करके कि वह पुनर्जन्म चाहता है या उसे टालना चाहता है, देह त्याग करनी होती है।
अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।। २४ ।।
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ।। २५ ।।
२४-२५. अग्नि एवं प्रकाश तथा धुँआ अथवा धुँध, दिन एवं रात, महीने का शुक्लपक्ष एवं कृष्णपक्ष, उत्तरायण एवं दक्षिणायन ये परस्पर विलोम चीजें हैं। इन विपर्ययों में प्रत्येक में से प्रथम विपर्यय के द्वारा ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं; परंतु दूसरे विपर्ययों के द्वारा योगी 'चंद्र के प्रकाश' को प्राप्त करता है और उसके बाद पुनः मानव जन्म में लौट आता है।
शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते ।
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ।। २६ ।।
२६. ये दो चिरस्थायी प्रकाशमय और अंधकारमय मार्ग हैं; इनमें से एक के द्वारा वह प्रयाण करता है जो पुनः लौट कर नहीं आता, और दूसरे से वह जो पुनः लौटता है।
नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।। २७ ।।
२७. हे पृथापुत्र! जो योगी इन दोनों मार्गों को जाननेवाला है वह कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिये हे अर्जुन सभी कालों में (हर समय) योगयुक्त हो।
(शुक्ल-कृष्ण गति की धारणा' के पीछे) चाहे जो मानस-भौतिक वास्तविकता हो या कोई प्रतीक हो - यह धारणा उन गुह्यवादियों के युग से चली आ रही है जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ में आंतरिक तत्त्व के प्रभावशाली प्रतीक को देखते थे और जो सर्वत्र ही बाह्य और आभ्यंतर, प्रकाश और ज्ञान, अग्नि-तत्त्व और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच परस्पर क्रिया तथा एक प्रकार की समरूपता देखते थे, - हमें तो केवल उस मोड़ को देखने की आवश्यकता है जिससे गीता इन श्लोकों का उपसंहार करती है: 'अतएव, सभी समय योगयुक्त रहो।'
क्योंकि अंततः यही मूलभूत बात है, संपूर्ण सत्ता को भगवान् के साथ एकात्म कर देना, इतने पूर्ण रूप से और सभी तरह से एकात्म कर देना कि यह स्वाभाविक और सतत् रूप से ऐक्य अवस्था में स्थित हो जाए, और इस प्रकार संपूर्ण जीवन, केवल विचार और ध्यान ही नहीं, अपितु कर्म, श्रम, युद्ध सब कुछ भगवान् का ही स्मरण बन जाए। 'मामनुस्मर युद्धय च', 'मेरा स्मरण कर और युद्ध कर', अर्थात् इस अनित्य पार्थिव संघर्ष में, जो सामान्यतः हमारे मन को ग्रसित किये रहता है, क्षण भर के लिए भी शाश्वत के सतत् चिंतन को न छोड़ देना; और यह बात बहुत ही कठिन, प्रायः असंभव ही प्रतीत होती है। वस्तुतः यह सर्वथा संभव तभी होती है जब इसके साथ अन्य शर्तें भी पूरी हों।
----------------------------------------------
• योग का अनुभव वस्तुतः यह दिखाता है कि इस धारणा के पीछे एक यथार्थ मनोभौतिक सत्य है, अवश्य ही यह हर जगह पूर्ण या निरपेक्ष रूप से व्यवहार्य नहीं है, इस धारणा के पीछे की युक्ति यह है कि, प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के बीच जो आंतरिक युद्ध होता है उसमें प्रकाश की शक्तियों का दिन या वर्ष के प्रकाशमय समयों में स्वाभाविक प्राधान्य रहता है और अंधकार की शक्तियों का अंधकारमय समयों में, और यह संतुलन तब तक चलता रह सकता है जब तक कि अंतिम विजय प्राप्त नहीं हो जाती।
हमारे शाखों में जगह-जगह ऐसा वर्णन आता है कि रात्रि के समय राक्षसों की, आसुरी शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है। और ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं की ताकत बढ़ जातो है। हमारा सारा ज्योतिषशास्त्र, शकुन शास्त्र आदि इन्हीं भौतिक, सूक्ष्म भौतिक और मनो-भौतिक संकेतों, प्रतीकों आदि पर आधारित हैं। पशु-पक्षियों की, कीड़े-मकोड़ों की आवाजें, व्यवहार आदि के आधार पर भी पूरा शास्त्र आधारित है क्योंकि उनके व्यवहार आदि से बहुत से भौतिक तथा सूक्ष्म संकेत प्राप्त होते हैं। हालांकि इन सब में सदा ही कोई अप्रत्याशित तत्त्व तो रहता ही है परंतु फिर भी ये सारे संकेत बहुत हद तक हमें चीजों के विषय में निश्चित पूर्वाभास प्रदान करते हैं। पूर्वकाल में हम राजा-महाराजाओं की कथाओं में देखते हैं कि किस प्रकार जन्म के समय ही राजज्योतिषी बच्चे का लगभग सटीक भविष्य बता देते थे। और कुछ मामलों में तो वह भविष्यकथन अक्षरशः सही होता था।
यदि हम अपनी चेतना में सबके साथ एक आत्मा हो चुके हैं - वह एक आत्मा जो सदा हमारी बुद्धि में स्वयं भगवान् हैं, और यहाँ तक कि हमारे नेत्र तथा अन्य इन्द्रियाँ इन्हीं भगवान् को सर्वत्र इस प्रकार देखती और अनुभव करती हैं कि किसी भी समय किसी भी पदार्थ को हम वैसा नहीं अनुभव करते या समझते जैसा कि असंस्कृत बुद्धि और इन्द्रियाँ अनुभव करती हैं, अपितु उसे उस रूप में छिपे हुए तथा साथ-ही-साथ उस रूप में प्रकट होनेवाले भगवान् ही जानते हैं, और यदि हमारी इच्छा भगवदिच्छा के साथ चेतना में एक हो चुकी है और हमें अपनी इच्छा, अपनी मन-बुद्धि और शरीर का प्रत्येक कर्म उसी भगवदिच्छा से निःसृत, उसी का एक प्रवाह, उसी से भरा हुआ या उसके साथ एकीभूत प्रतीत होता है तो गीता की जो माँग है उसे सर्वांगीण रूप से किया जा सकता है। अब भगवत्स्मरण मन की रुक-रुक कर होनेवाली कोई विशेष क्रिया नहीं होती, अपितु हमारे क्रियाकलापों की सहज स्थिति और एक तरीके से चेतना का सारतत्त्व मात्र ही बन जाता है। अब जीव पुरुषोत्तम के साथ अपना यथार्थ, स्वाभाविक एवं आध्यात्मिक संबंध प्राप्त कर चुका होता है और हमारा संपूर्ण जीवन एक योग बन गया है, वह योग जो सिद्ध होने पर भी शाश्वत रूप से और अधिक आत्म-सिद्ध होती एकता बनता जाता है।
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ।। २८ ।।
२८. वेदों में, यज्ञानुष्ठानों में, तपों में तथा दानों में जो पुण्यकमर्मों का फल बताया गया है, इसको जानकर योगी इन सबसे परे चला जाता है और परम् और नित्य पद प्राप्त करता है।
इस प्रकार आठवाँ अध्याय 'अक्षरब्रह्मयोग' समाप्त होता है।
नवाँ अध्याय
I. राजगुह्य
समस्त सत्य जिसने अपने-आप को यहाँ तक क्रमशः विकसित किया है, जो प्रत्येक सोपान पर समग्र ज्ञान के किसी नवीन पहलू को प्रस्तुत करता आया है और उस पर आध्यात्मिक अवस्था और कर्म के किसी-न-किसी निष्कर्ष को स्थापित करता गया है, उसे अब एक ऐसा मोड़ लेना है जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसलिए भगवान् आगे जो कुछ कहनेवाले हैं उसके निर्णायक स्वरूप की ओर पहले ही ध्यान दिला देते हैं जिससे कि अर्जुन का मन जागृत और सतर्क हो सके। क्योंकि वे उसका मन समग्र भगवत्ता के ज्ञान और दर्शन के प्रति खोलने वाले हैं और ग्यारहवें अध्याय के उस विराट् दर्शन तक ले जाने वाले हैं, जिससे कि कुरुक्षेत्र का यह योद्धा अपनी सत्ता, कर्म और विशिष्ट कार्य के उन रचयिता और धर्ता के प्रति, मनुष्य और जगत् में व्याप्त भगवान् के प्रति सचेतन हो जाए जिन्हें मनुष्य में और संसार में कोई चीज सीमित या बद्ध नहीं करती, क्योंकि सभी कुछ उन्हीं से निःसृत है, उन्हीं की अनन्त सत्ता में एक गतिविधि है, उन्हीं की इच्छा से यह जारी रहता है और उसी के द्वारा आश्रित रहता है, उन्हीं के दिव्य आत्मज्ञान में इसकी सार्थकता सिद्ध होती है, वे ही सदा इसके आदि, सार और अंत हैं। अर्जुन को अपने बारे में यह जानना होगा कि वह केवल उन्हीं भगवान् में अस्तित्वमान रहता है और अपने अंदर केवल उन्हीं की शक्ति के द्वारा कार्य करता है, उसके समस्त क्रियाकलाप भागवत् क्रिया का एक साधनमात्र हैं, उसकी अहंपरक चेतना केवल एक आवरण है और उसके अज्ञान के लिए वह उसकी अंतःस्थित सच्ची सत्ता का, जो कि परम् पुरुष परमेश्वर का अमर स्फुल्लिंग और अंश है, मिथ्या प्रतिभास मात्र है।
यही सत्य सत्ता का रहस्य है जो कि अब गीता इसकी प्रचुर फलवत्ता के साथ हमारे आंतरिक जीवन और बाह्य कर्मों के लिए प्रयुक्त करने जा रही है। वह जो अब कहने जा रही है वह गुह्यतम रहस्य है। यह समग्र भगवान्, समग्र माम्, का वह ज्ञान है जिसे अर्जुन को उसकी सत्ता के प्रभु ने देने का वचन दिया है, वह मूलभूत ज्ञान जो सभी तत्त्वों में (भगवत्ता के) पूर्ण ज्ञान से युक्त है, जो फिर और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रख छोड़ता। अज्ञान की वह संपूर्ण ग्रंथि जिसने उसकी मानव-बुद्धि को भ्रमित किया है और जिसने उसके संकल्प को अपने भगवद्-नियत कार्य से पीछे हटा दिया है, वह (इस मूलभूत ज्ञान द्वारा) पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न हो चुकी होगी। यह सब ज्ञानों का ज्ञान, सब गुह्यों का गुह्य, राजविद्या, राजगुह्य है।
इस नवें अध्याय में भगवान् की सत्ता का मोटा-मोटा सारा निरूपण आएगा कि किस प्रकार सभी कुछ भगवान् स्वयं ही हैं। उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उन्हीं से सभी चीजों का उद्गम है, उन्हीं से उनकी गति और उन्हीं में उनका लय है। इस निरूपण में पहले तो कुछ पहेलीनुमा बातें आती हैं जैसे कि 'मैं सभी भूतों में स्थित हूँ परंतु समस्त भूत मुझमें स्थित नहीं हैं।' चूंकि ये सभी बातें पहेलीनुमा हैं इसलिए अपने आप में स्थूल होने के कारण बुद्धि इन बातों से चकरा जाती है इसलिए उसे सूक्ष्म बनाना, परिष्कृत करना आवश्यक है।
श्रीभगवान् उवाच
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ।। १।।
१. श्रीभगवान् ने कहाः तुझ दोषदृष्टि-रहित को जो / अब कहने जा रहा हूँ, वह गुह्यतम चीज है, वह मूलभूत ज्ञान है जो समस्त व्यापक ज्ञान (विज्ञान) से युक्त है, जिसे जान कर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा।
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धम्यै सुसुखं कर्तुमव्ययम् ।। २।।
२. यह राजविद्या है, राजगुह्य (सभी रहस्यों में रहस्य) है, यह पवित्र और उच्चतम कोटि का प्रकाश है जिसका आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा सत्यापन किया जा सकता है, सत्ता का सही धर्म है, जिसका अभ्यास करना सरल है और जो अविनश्वर है।
अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्र्मनि ।। ३।।
३. हे परंतप! इस धर्म में श्रद्धा न प्राप्त कर पाने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त करके सामान्य मर्त्य जीवनपथ में लौट आते हैं।
....यदि श्रद्धा न हो, यदि व्यक्ति उस तार्किक बुद्धि का ही भरोसा करता हो जो बाह्य तथ्यों के आधार पर चलती है और शंकालु दृष्टि से अन्तर्दृष्ट ज्ञान पर इस कारण संदेह करती है क्योंकि वह बाह्य प्रकृति के विभाजनों और अपूर्णताओं के साथ मेल नहीं खाता और उससे परे की चीज प्रतीत होता है तथा कोई ऐसी चीज व्यक्त करता प्रतीत होता है जो हमें हमारे वर्तमान जीवन के प्रथम व्यावहारिक तथ्यों से, इसके दुःख-दर्द से, पाप, दोष, भगवद्-विरुद्ध प्रमाद व स्खलन, अशुभ, से परे ले जाता है, तो फिर उस महत्तर ज्ञान से युक्त जीवन बिताने की कोई संभावना नहीं है। जो जीव उच्चतर सत्य और विधान में श्रद्धा नहीं ला पाता उसे अवश्य ही मृत्यु, दोष और अशुभ के अधीन सामान्य मर्त्य जीवनपथ में लौट आना पड़ता है: वह उन परमेश्वर के स्वरूप में विकसित नहीं हो सकता जिनकी सत्ता को वह नकारता है। क्योंकि यह एक ऐसा सत्य है जिसे जीना होता है, - और आत्मा के विकसित होते प्रकाश में जीना होता है, न कि मन के अंधकार में उसे तर्क द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। यदि व्यक्ति को भगवान् के वचनों में श्रद्धा आ गई है तो वह उन्हें जीने का प्रयास करेगा ही, जबकि जिसे उनके वचनों में श्रद्धा नहीं आई है वह तो अपनी सामान्य जीवनचर्या में ही निरंतर चलता रहेगा। हालाँकि श्रद्धा आने पर भी मन, बुद्धि आदि भाग तो सक्रिय ही रहते हैं, एकाएक ही वे परिवर्तित नहीं हो जाते। वे पूर्ववत् ही अपनी क्रिया करते रहते हैं और मन-बुद्धि की किसी भी क्रिया से, हमारे किन्हीं भी भौतिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक नियमों आदि से भगवान् के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता और न ही वे हमें भगवान् की ओर जाने के मार्ग में अग्रसर ही कर सकते हैं। श्रद्धा के आधार पर व्यक्ति मार्ग पर आरंभ तो कर सकता है परंतु कदम-कदम पर उसे जो व्यावहारिक निर्णय लेने होते हैं उनके लिए वही पुराना दृष्टिकोण, वही पुराने मन-बुद्धि और अधिक सहायक नहीं रहते। तब फिर व्यावहारिक निर्णय कैसे किये जाएँ? इसके लिए श्रीअरविन्द कहते हैं, "यह एक ऐसा सत्य है जिसे जीना होता है, - और आत्मा के विकसित होते प्रकाश में जीना होता है, न कि मन के अंधकार में उसे तर्क द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।" इसलिए व्यक्ति जब इस मार्ग पर चलता है और इस पर उसे जो भी कोई अनुभव प्राप्त होते हैं, भले कोई छोटा ही अनुभव क्यों न प्राप्त हुआ हो, तब वह अनुभव या वे अनुभव व्यक्ति को मस्तिष्क के समस्त क्रियाकलापों से, विज्ञान के सभी नियमों से, सभी दर्शनों से, साधना के सभी नियमों से कहीं अधिक प्रकाश प्रदान करते हैं। इसलिए इस अध्याय के आरंभ में ही गीता श्रद्धा के ऊपर और आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर सत्य के सत्यापन पर बल देती है क्योंकि अन्य किन्हीं भी साधनों से इस सत्य का सत्यापन नहीं हो सकता। अतः जैसे-जैसे व्यक्ति को अधिकाधिक अनुभव प्राप्त होते जाएँगे वैसे-वैसे उसे और अधिक मार्गदर्शन प्राप्त होता जाएगा। यदि मानसिक स्तर पर ही गहरे सत्यों के रहस्य को समझा जा सकता हो तब तो बुद्धिजीवियों द्वारा बहुत पहले ही इस रहस्य को समझा जा चुका होता। परंतु यह राजगुह्य है जिसकी ओर व्यक्ति को श्रद्धा के आधार पर चलना होता है जो कि अनुभव लाती है और उस अनुभव से आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी कारण आध्यात्मिक पथ पर गुरु के मार्गदर्शन की परम आवश्यकता रहती है क्योंकि विरला ही कोई होता है जो अपनी निज शक्ति-सामर्थ्य से इस निम्न क्रियाकलाप से, अपरिष्कृत बुद्धि की क्रिया से ऊपर उठ सके। हालाँकि ज्यों-ज्यों व्यक्ति पथ पर अग्रसर होता है त्यों-त्यों उसकी बुद्धि भी अधिक परिष्कृत होती जाती है और अभिव्यक्ति में उसकी सहायता करती है। चूंकि व्यक्ति को आगे से आगे अनुभव प्राप्त होते जाते हैं तो उनकी सहायता से मनुष्य की बुद्धि, उसके भाव, उसका दृष्टिकोण आदि सब बदलते जाते हैं। यह नवाँ अध्याय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भगवान् इसमें अपने गुह्य तत्त्व का, अपने भगवत्तत्त्व का निरूपण करते हैं।
व्यक्ति को उसी में विकसित होना होता है, वही हो जाना होता है, - उसकी सत्यता परखने का या सिद्ध करने का केवल यही तरीका है। केवल निम्नतर सत्ता को अतिक्रम करके ही कोई सच्ची दिव्य सत्ता बन सकता है और आत्मिक जीवन के सत्य को जी सकता है। सत्य के जितने भी आभास इसके विरोध में प्रस्तुत किये जाएँ, वे सब निम्न प्रकृति की ही प्रतीतियाँ हैं। निम्न प्रकृति के इस अशुभ से मुक्ति उस उच्चतर ज्ञान को ग्रहण करने से ही आ सकती है जिसमें यह प्रत्यक्ष या भासमान अशुभ अपने स्वरूप की चरम अयथार्थता स्वीकार कर लेता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह हमारे अंधकार की सृष्टि थी। पर इस प्रकार दिव्य 'प्रकृति' के मुक्त भाव की ओर विकसित होने के लिए हमें हमारी वर्तमान सीमित प्रकृति में निगूढ़ परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करना होगा व उसमें विश्वास करना होगा। क्योंकि जिस कारण से यह योग संभव और सहज हो जाता है वह यह है कि इसे साधने में हम जो स्वाभाविक रूप से हैं उस सब की क्रियाओं को उन अंतःस्थ दिव्य पुरुष के हाथों में सौंप देते हैं। भगवान् हमारी सत्ता अपनी सत्ता में मिलाकर और उसे अपने ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण कर, 'ज्ञानदीपेन भास्वता', सहज, अचूक रीति से हमारे अन्दर उत्तरोत्तर दिव्य जन्म साधित कराते हैं: वे हमारी तमसाच्छा अज्ञानमयी प्रकृति को अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने प्रकाश औ व्यापक भाव में रूपान्तरित कर देते हैं। हम जिस पर पूर्ण श्रद्धा के साथ औ अहंकार-रहित होकर दृढ़ विश्वास करते हैं और उनके द्वारा प्रेरित होकर होन चाहते हैं, उसे अंतःस्थ भगवान् निश्चय ही सिद्ध कर देंगे। परंतु पहले अहंभावापर मन और प्राण को, जो कि हम वर्तमान में हैं और बाह्यतः प्रतीत होते हैं, अपने रूपांतरण हेतु स्वयं को हमारे अंतःस्थ अंतरतम गूढ़ भगवत्ता के हाथों में समर्पित करना होगा।
x.11
तीसरे श्लोक में भगवान् कहते हैं कि, "हे परंतप ! इस धर्म में श्रद्धा न प्राप्त कर पाने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त करके सामान्य मर्त्य जीवनपथ में लौट आते हैं।" यह उक्ति परम महत्त्व की है। क्योंकि सभी कुछ उस मूलभूत श्रद्धा पर निर्भर करता है। सामान्यतः हम सुनते ही हैं कि हमें भगवान् पर विश्वास है। परंतु वास्तव में वह विश्वास भी हमारी सत्ता के किसी-किसी भाग में ही होता है और वह भी इतने क्षीण रूप से होता है कि उसमें हमारी सत्ता की ऊर्जाओं को, उसकी वृत्तियों को भगवान् की ओर मोड़ने की शक्ति नहीं होती। हालाँकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें कि कोई गहरी चीज न हो, परंतु महत्त्व इस बात का है कि उसकी बाहरी सक्रिय प्रकृति पर उसका कितना प्रभाव है। इसी कारण सत्संग का, धर्मग्रंथों का, भजन-कीर्तन आदि का, सत्पुरुषों के पास जाने का, तीर्थों में जाने का इतना भारी महत्त्व है। क्योंकि यों तो सभी कुछ होता तो परमात्मा की ही इच्छा से है परंतु व्यक्ति की बाहरी प्रकृति का गठन जिस प्रकार का है, उसमें ये सभी बाहरी साधन अन्दर की श्रद्धा को जागृत करने में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसी चीजों के संपर्क में भीतरी श्रद्धा को जागृत होने का अधिकतम सुअवसर प्राप्त होता है। और जब वह श्रद्धा बाहरी प्रकृति तक भी अपना प्रभाव डालने में, व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन को भी नियोजित करने में समर्थ होती है तब व्यक्ति योग की ओर उन्मुख हो जाता है अन्यथा तो वह साधारण जीवन ही व्यतीत करता रहता है। अतः जो इस श्रद्धा को प्राप्त नहीं कर सकता वह भगवान् की ओर नहीं जा सकता। भले व्यक्ति कितने भी तकों से भगवान् की सत्ता को मंडित करने का या उसे अस्वीकार करने का प्रयास करे, परंतु केवल श्रद्धा के द्वारा और उसके प्रभाव से मार्ग पर होने वाले सतत् वर्धित होते अनुभवों के द्वारा ही वह वास्तव में उस ओर बढ़ सकता है और केवल तभी मार्ग पर आने वाली समस्याओं का, सभी प्रकार के संशयों आदि का सच्चे रूप से समाधान हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या संदेह, संशय आदि निरर्थक हैं? परंतु सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी कि अपने सही समय और स्थान पर उपयोगिता न हो। श्रद्धा जब अपने आप को विभिन्न भागों के द्वारा प्रकट करती है तब हमारे मन, प्राण और शरीर आदि भाग इतने सक्षम नहीं होते कि वे सही रूप में, बिना किसी प्रकार की त्रुटि या विकृति के उसे ग्रहण कर सकें और अभिव्यक्त कर सकें। हमारी बाह्य प्रकृति आरंभ में बहुत ही अपरिष्कृत, तुच्छ, अनमनीय और क्षुद्र होती है और बड़े ही सतत् अभ्यास के द्वारा उसका विकास होता है। और ज्यों-ज्यों उसका विकास होता है त्यों-त्यों वह उस श्रद्धा को अधिकाधिक सही रूप में ग्रहण कर सकती है और अभिव्यक्त कर सकती है। इसलिए हमारी बाह्य चेतना अपरिपक्व होने के कारण उसमें श्रद्धा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता इसलिए उसमें संशय और संदेह उपयोगी होते हैं ताकि हम श्रद्धा के उस अपूर्ण प्रतिबिंब को ही अंतिम न मान बैठें और उसी में रूढ़ न हो जाएँ। यदि व्यक्ति में संशय न उठते तब तो वह अपनी किसी भी प्रकार की धारणा को, सनक को, पूर्वाग्रह को ही सही मानकर उसी के अनुसार चलने लगेगा जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है। और यह चीज इतनी आम है कि प्रायः ही हम लोगों को प्रेरणा के नाम पर, भीतरी श्रद्धा के नाम पर अतियों में लिप्त होते देखते हैं। इसलिए अपने आप में श्रद्धा पर नहीं बल्कि मन-बुद्धि आदि भागों में उसके निरूपण पर संदेह अत्यंत आवश्यक है। इस बात में संशय नहीं करना है कि गंतव्य तो परम प्रभु ही हैं, क्योंकि यह तो आत्मा का सहज सत्य है, सच्ची श्रद्धा है, परंतु यह श्रद्धा व्यावहारिक जीवन में अपने आप को किस रूप में अभिव्यक्त करती है उन रूपों पर मनुष्य को संशय या संदेह होना आवश्यक है ताकि वह बाहरी भागों की त्रुटियों, विकृतियों आदि की रोकथाम कर सके जिससे कि उस श्रद्धा को अधिक शुद्ध रूप में अभिव्यक्त किया जा सके। और श्रद्धा एक इतना महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो व्यक्ति को भगवान् की ओर ले जाता है। इसीलिए गीता आर्त्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु आदि सभी भक्तों को श्रेष्ठ बतलाती है क्योंकि महत्त्वपूर्ण चीज है किसी भी प्रकार भगवान् की ओर चलना, उनसे संबंध स्थापित करना और अधिकाधिक उन्हें जीवन में अभिव्यक्त करना। और जब एक बार व्यक्ति किसी भी भाव से भगवान् की ओर चल पड़ता है तब उसके अशुभ नष्ट हो जाते हैं।
प्रश्न : भगवान् कहते हैं कि, "इस धर्म में श्रद्धा न प्राप्त कर पाने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त करके सामान्य मर्त्य जीवनपथ में लौट आते हैं।" तो वह किस धर्म के विषय में है?
उत्तर : सामान्य अर्थ में जिसे हम धर्म समझते हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है। भगवान् कहते हैं कि यह राजगुह्य, जिसका कि आध्यात्मिक अनुभव से ही सत्यापन किया जा सकता है, सत्ता का सही धर्म है। और राजगुह्य और कुछ नहीं केवल यह रहस्य है कि भगवान् ही सब कुछ हैं और जीवन में उन्हें चरितार्थ करना ही एकमात्र सच्चा उद्देश्य है, यही सच्चा धर्म है। और जिसे इस धर्म में, इस राजगुह्य में श्रद्धा आ गई है वह तो अवश्य ही अपने गंतव्य की ओर चला जाएगा। इसलिए भले तकलीफ में ही सही, भले किसी स्वार्थ के कारण या फिर जिज्ञासावश ही सही, पर यदि किसी प्रकार भी व्यक्ति को भगवान् की सत्ता में विश्वास आ गया कि उन्हीं के पास जाना चाहिये, तब व्यक्ति बिल्कुल सही भाव में है। और बिना इस विश्वास के तो भक्ति का कोई आधार ही नहीं है। जिसकी सत्ता मात्र को व्यक्ति स्वीकार न करता हो उसको भक्ति वह कर ही कैसे सकता है। इसलिए यह विश्वास भक्ति का प्राथमिक आधार बन जाता है।
प्रश्न : पहले श्लोक में भगवान् कहते हैं कि तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो अशुभ क्या है?
उत्तर : जो कुछ हमें परमात्मा की ओर जाने से रोकता है वही अशुभ है। अपने आप में कोई चीज शुभ या अशुभ नहीं होती। यह तो देश-काल और पात्र पर निर्भर करता है कि कौनसी चीज भगवान् की ओर जाने में सहायक हो जाती है और कौनसी बाधक। किसी अमुक अनुभव से व्यक्ति भगवान् को ओर जा सकता है और किसी अमुक अनुभव में व्यक्ति फँस भी सकता है। हालाँकि सामान्यतया कुछ चीजें शुभ ही मानी जाती हैं, जैसे कि भगवान् के प्रेमीजनों का संग, सत्पुरुषों का संग। इसमें यह अपवाद अवश्य हो सकता है कि यदि स्वयं उस व्यक्तिविशेष की अवस्था ही इतनी ऊँची हो कि उसे उन तथाकथित सत्पुरुषों के साथ मेलजोल करने में सतर्क भी रहना पड़े। परतु यह तो अत्यंग विरले प्रसंगों में ही होता है। स्वयं श्रीअरविन्द ने कहा कि उन्हें श्रीमाताजी के आने से पूर्व पांडिचेरी में अन्य किसी से कभी कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न चीजें होती है। परंतु मुख्न बात है कि यदि भगवान् के प्रति वह श्रद्धा आ जाए तो व्यक्ति उनकी ओर गति करना आरंभ कर देता है पर यदि वह जागृत न हो तो केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, वास्तविक कोई गति होती नहीं। पर एक बार जब भगवान् को ओर कदम बढ़ जाएँ तो फिर देर-सवेर, कितने भी उतार-चढ़ावों से होते हुए व्यक्ति अंततः गंतव्य तक पहुँच ही जाता है। इसीलिए भगवान् कहते हैं कि 'सन्मुख होई जीव मोहिं जबहि, जनम कोटि अघ नासहिं तबहिं।'
प्रश्न : जब एक बार व्यक्ति उस राह पर कदम बढ़ा देता है तब क्या पीछे जाने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है?
उत्तर : हमारे प्राण का खेल बड़ा ही भयंकर और खतरनाक है। इसीलिए तो गीता छठे अध्याय के तेईसवें श्लोक में कहती है कि 'इस योग का चित्त में किसी भी प्रकार के अनुत्साह अथवा विषाद में डूबे बिना दृढ़तापूर्वक निरंतर अनुष्ठान करना चाहिए।' इसी पर टिप्पणी करते हुए श्रीअरविन्द कहते हैं, "...हृदय तथा मन की अधीरता और हमारी राजस प्रकृति की उत्सुक पर स्खलनशील इच्छा-शक्ति के कारण योग के विषम तथा संकीर्ण पथ पर इस श्रद्धा तथा धैर्य की प्राप्ति करना अथवा उसका अभ्यास करना कठिन होता है। मनुष्य की प्राणिक प्रकृति सदा ही अपने परिश्रम के फल के लिये तरसती है और यदि उसे ऐसा लगता है कि फल देने से इंकार किया जा रहा है या इसमें बहुत देर लगायी जा रही है तो वह आदर्श तथा नेतृत्व में विश्वास खो बैठती है। क्योंकि, उसका मन सदा ही पदार्थों की बाह्य प्रतीति के द्वारा ही निर्णय करता है, क्योंकि यह उस बौद्धिक तर्क की पहली सबसे भारी गहराई तक जमी हुई आदत है जिसमें वह इतने अतिशय रूप से विश्वास करता है। जब हम चिरकाल तक कष्ट भोगते या अन्धेरे में ठोकरें खाते हैं तब अपने हृदयों में भगवान् को कोसने से अथवा जो आदर्श हमने अपने सामने रखा है उसे त्याग देने से अधिक आसान हमारे लिये और कुछ नहीं होता।...ऐसी घड़ियों में - और कभी-कभी ये बारम्बार आती हैं और दीर्घकालिक होती हैं समस्त उच्चतर अनुभव विस्मृत हो जाता है और हृदय अपनी कटुता में डूब जाता है, उसी पर केंद्रित हो जाता है। इन्हीं अंधकारमय कालों में यह आशंका रहती है कि हम सदा के लिये पतित हो सकते हैं अथवा दिव्य कार्य या श्रम से पराङ्गमुख हो सकते हैं।" (CWSA 23, 244) श्रीमाताजी इस विषय में चेतावनी देती हुई कहती हैं कि, "...जब तुम पथ पर होते हो, तो कभी भी उसका परित्याग न करो। कुछ प्रतीक्षा करो, पथ को स्वीकार करने से पूर्व तुम चाहो उतनी देर सकुचा सकते हो; परंतु जिस क्षण से तुम उस पर पदार्पण करो, तो बस, उसे छोड़ो मत। क्योंकि इसके परिणाम हैं जो अनेक जन्मों तक असर डाल सकते हैं। यह बहुत ही गंभीर है। इसीलिए सब कुछ के बावजूद योग पथ पर प्रवेश करने के लिए मैं कभी किसी को बाध्य नहीं करती।"
(CWM 4, 444)
योगी श्रीकृष्णप्रेम ने भी संदेह के कालों का वर्णन करते हुए बताया है कि किस प्रकार उन कालों में हमारे विभिन्न भाग श्रद्धा में विश्वास खो बैठते हैं और स्वयं अपने उस आधार तक को ही नष्ट-भ्रष्ट करने पर आमादा हो जाते हैं जो उन्हें थामकर आगे ले जा रहा था। श्रीकृष्णप्रेम ने इसका एक रूपक कथा के रूप में जो चित्रण किया है वह बड़ा ही हृदयस्पर्शी है। वे लिखते हैं, "मैंने कुंठित कामना के गहरे मंद स्वर को मानसिक समुद्र में प्रचण्ड रूप से दौड़ते देखा। विशाल लहरों में उसे मैंने सतह पर आते देखा, और मन के जहाज को, जिसके तार कटे हुए थे, घनघोर हवा के सामने भागते देखा। मैंने जहाजी दल को, जिनका भय उफनती लहरों के संपर्क के कारण आतंकित क्रोध में बदल गया था, अपनी कुल्हाड़ियाँ लेते और रस्सों और खंभों को बड़ी बेरहमी से काटते देखा। मैंने उन्हें अद्भुत दिशासूचक (compass) पर प्रहार करते देखा जो कि जहाज के बीचों-बीच प्रकाश से जगमग कर रहा था, यद्यपि उन्होंने दिशासूचक के कार्ड को तो नष्ट कर दिया था परंतु उसके प्रकाशपूर्ण काँटे को छू नहीं पाए। और अंत में वे अत्यंत उत्तेजित और क्रोधित हो गए और जहाज के लट्टे तक को ही चीर दिया और जब वह पानी में डूब गया तो वे भी कोसते और सुबकते हुए डूबने लगे। और फिर भी दिशासूचक चमक रहा था, एक आग्नेय काँटा जो समुद्र के ऊपर अंधेरे शून्य में बड़े शांत-स्थिर भाव से बना हुआ था। और जब उन्होंने उसे देखा तो वे उसकी ओर तैर कर गए और उसे पकड़ा, और तब मैंने देखा कि उनके चारों ओर एक बार फिर वह जहाज था, अपने सभी खंभों और लट्ठों के साथ यथावत् और अंधकारमय तूफान कहीं दूर गर्मियों के-से समुद्र के तले लुप्त हो गया था। परंतु दल के हृदयों में शर्मिंदगी भरी थी।" (योगी श्रीकृष्णप्रेम, लेखक दिलीप कुमार राय, प्रकाशक श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट, पृष्ठ ३६)
श्रीअरविन्द इसे विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति साधना के मार्ग पर कदम रखता है तब श्रद्धा को कुछ राशि के साथ ही साथ उसके अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, अपनी जानकारियों की राशि आदि होते हैं। परंतु साधना में ऐसे समय आते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि जिस श्रद्धा से उसने आरंभ किया था, जिस इष्ट या उद्देश्य के प्रति उसने अपने जीवन को अर्पित कर दिया था, उसने उसे संकट में अकेला छोड़ दिया है और उसने वृथा ही अपना जीवन किसी ऐसी चीज के पीछे लगा दिया जिसे उसको कोई परवाह ही नहीं है या जो संकटकाल में उसकी कोई सहायता नहीं करती, उसकी करुण पुकार नहीं सुनती। बहुत से ऐसे आस्तिक लोगों के हमें उदाहरण पढ़ने-सुनने को मिलते हैं जो आरंभ में बहुत अधिक धर्मपरायण थे और बहुत पूजा-पाठ आदि करते थे, परंतु किसी अत्यंत अप्रिय घटना के बाद वे भगवान् में अपना विश्वास खो बैठे। साधनामार्ग में भी हमें ऐसे लोगों के उदाहरण मिलते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपना सर्वस्व दाँव पर लगा दिया तो भी अंततः उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसलिए साधना मार्ग की बजाय तो संसार के तौर तरीकों से चला जाए वही समझदारी है। इसी प्रकार जब हमारी रूपक कथा का जहाजी बेड़ा संकट में आता है तब उसे अपने जहाज पर विश्वास समाप्त हो जाता है और वह उसे नष्ट कर देना चाहता है। परंतु ऐसे ही कालों में पुराने मूल्य, पुरानी धारणाएँ आदि तो टूट जाती हैं और व्यक्ति पाता है कि एक कहीं अधिक विशाल धरातल - एक छोटे जहाज की अपेक्षा एक विशाल जहाज - उभर कर आता है जिसके आधार पर वह अपनी यात्रा को जारी रख सकता है। इसी प्रकार यह यात्रा आगे से आगे बढ़ती रहती है जिसमें समय-समय पर हमारे अंदर संशय उत्पन्न हो जाते हैं और यदि साधक उन कालों में से विजयी रूप से बाहर निकल आता है तो वह पाता है कि उसकी श्रद्धा पहले से कहीं अधिक विशाल हो जाती है, उसकी मनोवैज्ञानिक तथा प्राणिक संरचना कहीं अधिक लचीली, विशाल तथा अधिक समावेशी हो जाती है। ऐसे काल अधिकांश साधकों के जीवन में आते हैं। हालाँकि व्यक्ति के गठन पर निर्भर करता है कि उसके लिए ये काल कितने लंबे चलते हैं और कितने प्रायः आते हैं। परंतु वास्तव में तो भले ही हमारा विश्वास कितना भी क्यों न डगमगाए, परंतु भगवान् सदा ही हमारी सहायता करते रहते हैं। यही दृढ़ आश्वासन प्रदान करने के लिए तो भगवान् अर्जुन को कहते हैं कि,
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।२:४०।।
इस मार्ग पर कोई भी प्रयास नष्ट नहीं होता, न ही कोई प्रत्यागमन ही होता है, इस धर्म का थोड़ा-सा अनुष्ठान भी महान् भय से मुक्त कर देता है।
इसलिए परमात्मा की ओर बढ़ाया हुआ एक कदम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। वहीं यदि कोई भगवान् के लिए कोई श्रम करता है, उनके निमित्त कोई कष्ट या पीड़ा उठाता है तब तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। व्यक्ति अपने अहं की पुष्टि के लिए, कामनाओं-वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने सगे-संबंधी, रिश्तेदारों के लिए तो सारे दिन अनेकानेक तकलीफें उठाता है परंतु भगवान् के लिए थोड़ा भी कष्ट उठाने का परम सुअवसर केवल किसी सौभाग्यशाली को ही मिलता है।
इसके बाद गीता परम और समग्र रहस्य को, उस एकमात्र चिंतन सत्य को जिसमें पूर्णता तथा मुक्ति के जिज्ञासू को रहना सीखना होगा, तथ उस रहस्य के सब आध्यात्मिक अंगों और उनके समस्त क्रिया-व्यापारों ओ पूर्णता के एकमात्र विधान को प्रकट करने की ओर अग्रसर होती है। यह पाय रहस्य उन परात्पर परमेश्वर का गूढ़ रहस्य है जो सब कुछ हैं और सर्वत्र हैं, श्री फिर भी जगत् तथा उसके नाना रूपों से इतने महत्तर और भिन्न हैं कि यह की कोई वस्तु उन्हें अपने में समाहित नहीं रखती, कोई वस्तु उन्हें वास्तविक रूप में व्यक्त नहीं करती, और कोई भी भाषा, जो देश और काल और उनके परस्पर सम्बन्धों से निर्मित पदार्थों के बाह्य रूपों से ली गई हो, उनके अचिन्त स्वरूप का किसी प्रकार संकेत नहीं कर सकती। परिणामतः, हमारी पूर्णता का विधान है हमारी संपूर्ण प्रकृति की उसके दिव्य स्रोत और स्वामी के प्रति आराधना और उन्हीं को आत्मसमर्पण। हमारा एकमात्र चरम मार्ग यही है कि जगत् में हमारे संपूर्ण अस्तित्व को, केवल किसी इस या उस अंश को हो नहीं, शाश्वत पुरुष की ओर एकांतिक गति में मोड़ दिया जाए। दिव्य योग को शक्ति और उसके गूढ़ रहस्य के द्वारा हम उनकी अनिर्वचनीय गुह्यताओं से निकल कर लौकिक पदार्थों की इस बद्ध प्रकृति में आ गये हैं। उसी योग की एक विपरीत गति के द्वारा हमें अवश्य बाह्य प्रकृति की सीमाओं को अतिक्रम करना होगा और उस महत्तर चेतना को फिर से प्राप्त करना होगा जिसके द्वारा हम भगवान् में और परम शाश्वत में निवास कर सकें।
अतः, कोई भी विचार, कोई भाव, कोई सूत्र भगवान् के अचिन्त्य स्वरूप को कभी भी प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए एकमात्र करने योग्य कार्य है उनके प्रति आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण के द्वारा ही इसकी कोई संभावना है कि हम उनके स्वरूप के किसी अंश को कुछ समझ पाएँ, अन्य किसी तरीके से तो यह संभव ही नहीं है। इसलिए एकमात्र करने योग्य कार्य है कि किसी भी प्रकार अपने पूरे अस्तित्व को, अपनी संपूर्ण सत्ता को भगवान् की ओर मोड़ कर उनके हाथों में सौंप दिया जाए।
....भगवान् यह सारा जगत् जो कुछ है वह सब, और इस जगत् में जो कुछ है वह सब और इस जगत् से अधिक भी जो कुछ है वह सब हैं। गीता सर्वप्रथम भगवान् की विश्वातीत सत्ता पर बल देती है। क्योंकि, अन्यथा बुद्धि अपने सर्वोच्च लक्ष्य को चूक जाएगी और केवल विश्वमय सत्ता की ओर हो मुड़ी रहेगी या फिर जगत् में स्थित भगवान् की किसी आंशिक अनुभूति से हो आसक्त रहेगी। इसके बाद गीता भगवान् की उस विश्वसत्ता पर बल देती है जिसमें सब कुछ गति और कर्म करता है। क्योंकि यही जगत्प्रपंच का औचित्य है और वही विस्तृत आध्यात्मिक आत्म-बोध की स्थिति है जिसमें भगवान् अपने-आप को काल-पुरुष के रूप में देखते हुए अपना जगत्कर्म करते हैं। इसके बाद, गीता ने कुछ तीव्र बल के साथ भगवान् को मानव शरीर में दिव्य निवासी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया है। क्योंकि, वे सब भूतों में अंतर्यामी पुरुष हैं, और यदि अंतर्व्याप्त भगवत्ता को स्वीकार न किया जाए तो न केवल वैयक्तिक जीवन का भागवत् अभिप्राय ही समझ में नहीं आएगा, अपितु अपनी परम आध्यात्मिक भवितव्यता की ओर हमारी तीव्र इच्छा अपनी महत्तम शक्ति ही खो बैठेगी, और मानवता के अंदर आत्मा का आत्मा से परस्पर-सम्बन्ध क्षुद्र, अतिसीमित और अहंकारमय ही बना रहेगा। अन्ततः, गीता विस्तारपूर्वक विश्व में सभी पदार्थों में दिव्य अभिव्यक्ति पर बल देती है और जो कुछ भी है उस सब की उन्हीं एकमेव भगवान् की प्रकृति, शक्ति और ज्योति से उद्भूत होने की पुष्टि करती है। क्योंकि भगवद्-ज्ञान हेतु ऐसी दृष्टि भी अत्यंत आवश्यक है; इसी के ऊपर संपूर्ण सत्ता का और समस्त प्रकृति का भगवान् की ओर पूर्ण रूप से मुड़ना आधारित है...
x.12
परम् पुरुष परमेश्वर, विश्वचेतना के पीछे अक्षर आत्मा, मानव आधार में स्थित व्यष्टिगत-ईश्वर और विश्व-प्रकृति तथा उसके सब कर्मों और प्राणियों में गुप्त रूप से चेतन अथवा अंशतः आविर्भूत ईश्वर, ये सब एक ही सद्वस्तु, एक ही भगवान् हैं। परन्तु इस एक ही भगवद् सत्ता के ये जो विभिन्न भाव हैं इनमें से किसी भी एक भाव का जो यथार्थ वर्णन हम पूर्ण विश्वास के साथ कर सकते हैं उसे जब भगवद् सत्ता के अन्य भावों पर घटाने का प्रयत्न करते हैं तब वह वर्णन उलट जाता या उसका अभिप्राय बदल जाता है।... यह एक ऐसी बात है जिसे हमें गीता में स्पष्टतया देखनी होगी; एक ही सत्य के ये जो विभिन्न भाव सम्बन्ध-भेद और उसके प्रयोग-भेद से हुआ करते हैं, इनके लिए अपने विचार में अवकाश रखना होगा। अन्यथा हमें परस्पर विरोध' और विसंगति ही दिखाई पड़ेगी जहाँ कि ऐसी कोई विषमता है ही नहीं अथवा दिखने में पहेलीनुमा वचन लगते हैं उनसे अर्जुन की तरह हम भी भ्रमित है जाएँगे।
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।। ४।।
४. मेरे द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् मेरी सत्ता की अकथनीय गुह्यता में विस्तृत हुआ है; समस्त भूत मेरे भीतर स्थित हैं किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ।
भगवान् की परम् सत्ता अभिव्यक्ति के परे हैः उनकी सच्ची नित्य मूर्ति जड़तत्त्व में व्यक्त नहीं होती, न ही वह प्राण की पकड़ में आती है, न वह मन के द्वारा संज्ञेय या चिन्त्य है, अचिन्त्यरूप, अव्यक्तमूर्ति। हम जो देखते हैं वह तो केवल एक स्वरचित 'रूप' है, वह भगवान् का सनातन 'स्वरूप' नहीं है। जगत् से भिन्न ऐसा कोई या ऐसा कुछ है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो कल्पनातीत, अनिर्वचनीय रूप से अनन्त भगवत्ता है जो अनन्तता के विषय में हमारे विशालतम अथवा सूक्ष्मतम विचार लेशमात्र भी आभास प्राप्त कर सकें उससे भी परे है। पदार्थों का यह समस्त ताना-बाना जिसे हम जगत् का नाम दे देते हैं, गति की यह समस्त अतिविशाल राशि जिसकी हम कोई सीमाएँ नहीं बाँध सकते... उसे अपनी अनिर्वचनीय विश्वातीत गुह्यता पर प्रतिष्ठित इसी सर्वोच्च अनन्त सत्ता ने बुना है, रूप दिया है और विस्तारित किया है। यह एक ऐसे आत्म-निरूपण या आत्म-रूपायन पर प्रतिष्ठित है जो स्वयं अव्यक्त और अचिंत्य है। यह सदा परिवर्तनशील और गतिशील संभूति का समूह, ये सब जीव, भूत, पदार्थ, साँस लेते और जीवित रूप, ये सभी समूहगत रूप से या फिर अपनी पृथक् पृथक् सत्ता में भी उन भगवान् को समाहित नहीं कर सकते। वे (भगवान्) उनमें नहीं हैं; उनके अन्दर या उनके द्वारा नहीं जीते, चलते या अस्तित्वमान बने रहते हैं - भगवान् संभूति नहीं हैं। अपितु वे भूत आदि ही उनके अन्दर हैं, वे ही उनके अन्दर जीते, चलते और उन्हीं से अपने स्वरूप का सत्य प्राप्त करते हैं; भूत उनकी संभूति हैं और वे उनकी आत्मसत्ता हैं। अपनी सत्ता को अचिंत्य देश-कालातीत अनंतता में उन्होंने एक असीम देश और काल में एक असीम संसार का यह छोटा-सा दृश्य फैलाया है।
---------------------------------
• यह जगत् एक आध्यात्मिक विरोधाभास है,
जो 'अदृष्ट' के अंदर एक आवश्यकता द्वारा रचा गया है,
जो प्राणी के इन्द्रियबोध के लिए उस 'तत्' का
विरूपित रूप है, जो सदा विचार और वाणी से परे है,
उसका प्रतीक है जिसे कभी प्रतीक में व्यक्त नहीं किया जा सकता,
एक ऐसी भाषा जो अशुद्ध-उच्चारित, अशुद्ध-वर्तनी है,
परंतु है फिर भी सत्य।
जब भगवान् कहते हैं कि भूत उनमें स्थित हैं परंतु वे भूतों में स्थित नहीं हैं तो इसका वास्तव में अर्थ क्या है? हमारे वैदिक ऋषियों को इस बात का भली-भाँति ज्ञान था कि जो कुछ भी गोचर होता है वह आया तो परमात्मा से ही है अतः जिस प्रकार हम किसी धागे को उसके किसी एक छोर से पकड़ कर चलें तो दूसरे छोर तक पहुँच सकते हैं, उसी प्रकार यदि हम इस जड़ तत्त्व को पकड़ कर चलें तो इसके मूलस्रोत तक पहुँचा जा सकता है। यह तो एक तर्कसम्मत बात है कि चूँकि परमात्मा ने ही अधिकाधिक स्थूल बनते-बनते हमारा यह वर्तमान रूप धारण किया है इसलिए अवश्य ही इसके अधिकाधिक सूक्ष्म स्तरों पर जाने से हम पुनः स्रोत तक पहुँच सकते हैं। अतः सभी चीजें भगवान् में ही हैं। परंतु भगवान् उनमें नहीं हैं, इस बात को कैसे समझा जाए? इसका अर्थ है कि भगवान् की अभिव्यक्ति का हम जितना गहरे से गहरा, विशाल से विशाल अर्थ भी लगाएँ तो भी भगवान् का स्वरूप उसकी पकड़ में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि भगवान् इस सब में नहीं हैं, परंतु हम इसको जो कुछ भी समझते हैं, ऊँची से ऊँची चेतना के द्वारा भी हम इसका जो भी अर्थ लगा सकते हैं उसमें परमात्मा का एक क्षुद्र अंश भी पकड़ में नहीं आता। उनका स्वरूप तो अचिंत्य है। इसीलिए सारा निरूपण करने के बाद भी हमारे सद्ग्रंथ उनके स्वरूप के विषय में 'नेति नेति' ही कहते हैं। गीता भी उसी वैदिक सत्य को प्रतिध्वनित करती है कि भले ही सभी कुछ परमात्मा से ही निःसृत हुआ है, यही नहीं, बल्कि सभी कुछ परमात्मा स्वयं ही हैं परंतु फिर भी उससे परमात्मा को सीमित नहीं किया जा सकता। भले ही परमात्मा उस पदार्थ में हैं परंतु जिस दृष्टि से हम उन्हें उसमें देखते हैं उस दृष्टि से वे सीमित नहीं हो जाते। इस तरह से देखने से हमें दोनों विरोधाभासी प्रतीत होने वाली बातों के पीछे का औचित्य समझ में आने लगता है।
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।। ५।।
५. और फिर भी समस्त भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, मेरे दिव्य योग को देख; मेरा आत्मा समस्त भूतों का सृष्टिकर्ता और उनका धारक है, किन्तु उनमें स्थित नहीं है।
विश्वातीत परमेश्वर के नाते भगवान् भूतों में नहीं हैं, और न भूत उनमें हैं; क्योंकि आत्मसत्ता और भूतभाव में हम जो भेद करते हैं वह केवल दृश्य जगत् के अंदर अभिव्यक्ति पर ही लागू होता है। विश्वातीत सत्ता में सब कुछ शाश्वत आत्मसत्ता है और यदि वहाँ भी कोई बहुत्व हुआ तो, वे सब भी शाश्वत आत्मसत्ताएँ हैं। और न ही वहाँ देश में निवास करने का विचार ही उत्पन्न हो सकता, क्योंकि विश्वातीत निरपेक्ष सत्ता देश और काल की धारणाओं से, जो कि यहाँ प्रभु की योगमाया द्वारा रचे गए हैं, प्रभावित नह होती। कोई देश-काल मर्यादित नहीं अपितु एक आध्यात्मिक सह-अस्तिल एक आध्यात्मिक सारूप्य और सहस्थिति ही वहाँ मूल आधार होने चाहिए। परन्तु इसके विपरीत, वैश्विक अभिव्यक्ति में परम अव्यक्त विश्वातीत पुरुष के द्वारा देश और काल के अन्दर विश्व का विस्तार है, और उस विस्तार में पहले एक आत्मतत्त्व के रूप में प्रकट होते हैं जो 'भूतभृत्' है अर्थात् सर भूतों को धारण करता है, वह उन्हें अपनी सर्वव्यापक आत्मसत्ता में धारण करता है। और यहाँ तक कि, इस सर्वत्रव्यापी आत्मा के द्वारा परम् पुरुष परमात्मा भी इस जगत् को धारण किये हुए हैं ऐसा कहा जा सकता है, वे इसके अदृश्य आध्यात्मिक मूल और सब भूतों की अभिव्यक्ति के गुप्त आध्यात्मिक कारण हैं। वे जगत् को उसी प्रकार वहन किये हुए हैं जिस प्रकार हमारे अंदर की गुप्त आत्मा हमारे विचारों, कर्मों और गतिविधियों को वहन करती है। वे मन, प्राण और शरीर में व्याप्त होते और इन्हें अपने में समाहित रखते, उन्हें अपनी उपस्थिति से धारण करते हुए प्रतीत होते हैं: परन्तु स्वयं यह व्याप्ति चेतना की एक क्रिया है, भौतिक की नहीं; स्वयं शरीर केवल आत्मा की चेतना की ही एक सतत् क्रिया है।
प्रश्न : प्रभु की योगमाया का क्या अर्थ है?
उत्तर : जब हम कहते हैं कि प्रभु की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और केवल उन्हीं का ही अस्तित्व है और फिर भी हमें अपनी इंद्रियों आदि के माध्यम से बाहरी चीजों की जो प्रतीति होती है वही तो माया है। उदाहरण के लिए, यदि बहुत सारे समानांतर दर्पणों में किसी एक ही व्यक्ति के बहुत सारे प्रतिबिंब दिखने लगें और जिस व्यक्ति को दर्पण का ज्ञान न हो वह तो उन सब प्रतिबिंबों को देखकर भ्रमित ही हो जाएगा। कितने ही पशु-पक्षियों को हम देखते हैं जिन्हें दर्पण का ज्ञान नहीं होता और वे अपने ही प्रतिबिंब से लड़ते-लड़ते स्वयं को क्षति पहुँचाते हैं। वैसे ही, यदि व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त अपने परिवार, भाई-बहन, मित्र, आदि के मोह में फंसकर उनको यथार्थ समझ लेता है तो यह माया ही है। हमारे सारे शास्त्र यही बात कहते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी देखना माया है। इसीलिये भगवान् कहते हैं कि 'मम माया दुरत्यया' अर्थात् मेरी माया को कोई अतिक्रम नहीं कर सकता। केवल जो भगवान् की भक्ति करके उन्हें प्राप्त करते हैं वे ही उस माया से बच सकते हैं। यदि व्यक्ति यह सोचे कि वह किसी तरकीब से इस माया से बच जाएगा तो वह और भी अधिक माया में फँस जाता है इसलिए बिना भगवान् की भक्ति किए माया को कभी नहीं जीता जा सकता। एक कथा में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार अर्जुन ने भगवान् से उनकी माया दिखाने का आग्रह किया तो उन्होंने उसे अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। एक बार जब दोनों यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो अर्जुन ने पहले भगवान् को स्नान करने के लिए कहा। भगवान् ने स्नान किया और ऊपर आकर अपनी धोती बाँधते हुए उन्होंने अर्जुन को भी स्नान करने के लिए भेज दिया। अर्जुन जैसे ही जल के भीतर गया वैसे ही उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसे पकड़कर ले गए हैं और यमुना जी में ही उसे किसी देश का राजा बना कर उसका विवाह कर दिया है। इसके बाद अर्जुन ने वहीं सारे भोग-विलास किए और उसके भरा पूरा परिवार हो गया। और इस बीच उसने अन्य कई राजाओं से युद्ध कर उन्हें पराजित भी किया। इस तरीके से वह बहुत बड़ा शासक बन गया, और उसने अनेक यज्ञ आदि भी किए। एक दिन अचानक जब उसे भगवान् की याद आई तो वह यमुना जी से ऊपर आया और उसने देखा कि भगवान् तो अभी अपनी धोती ही बाँध रहे थे। तब भगवान् ने उसे समझाया कि यही माया है। न्यूनाधिक हम सभी के साथ भी यही है। हम अपने मूल स्वरूप को भूल बैठे हैं और इन प्रतीतियों को ही सत्य मानकर इन्हें अपना परिवार आदि कहकर इन्हीं में अतिशय रूप से आसक्त रहते हैं।
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।। ६॥
६. जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त महान् वायुतत्त्व आकाशतत्त्व में रहता है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझमें रहते हैं, इसको तुम्हें इस प्रकार समझना है।
यह दिव्य परमात्मा सभी भूतों को समाविष्ट रखता है; सभी उनमें अवस्थित हैं, वस्तुतः जड़ रूप से नहीं, अपितु आत्मसत्ता के उस विस्तृत आध्यात्मिक आधान के रूप में जिसके संबंध में एक भौतिक और आकाशीय विस्तार की हमारी अत्यंत सख्त या संकुचित धारणा उस तत्त्व का केवल भौतिक मन और इन्द्रियों की भाषा में अर्थ लगाना है। वास्तव में यहाँ भी सभी कुछ आध्यात्मिक सह-अस्तित्व, सारूप्य और सहस्थिति है; पर वह एक ऐसा मूलभूत सत्य है जिसे हम तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक कि हम उस परम चेतना तक पुनः नहीं जा पाते। तब तक ऐसा विचार केवल एक ऐसी बौद्धिक अवधारणा ही रहेगा जिससे हमारे व्यावहारिक अनुभव का मेल नहीं होता। अतः देश-काल में परस्पर संबंध के इन शब्दों का प्रयो मेल नहुए हमें कहना होगा कि यह जगत् और इसके सब प्राणी कि स्वतःस्थित सत्ता में वैसे ही रहते हैं जैसे अन्य सभी कुछ आकाश के के स्वतःरिश में रहता है.. आत्मा इन सब भूतों में या इनमें से किसी में भी का नहीं करती: कहने का अभिप्राय है कि, वह किसी पदार्थ द्वारा समाविष्ट से है, - ठीक वैसे ही जैसे आकाश यहाँ किसी रूप में समाविष्ट नहीं है, पद्म सभी रूप मूलभूत रूप से आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। और न ही वह सर्व भूतों के सम्मिलित रूप के द्वारा ही उनमें समाविष्ट या उनसे संघटित होती है। - ठीक वैसे ही जैसे आकाश वायुतत्त्व के गतिमान विस्तार के अन्दर समाचि नहीं होता न वायु के सब रूप या शक्तियाँ आकाश को संघटित ही का सकती हैं।
यहाँ बुद्धि के लिए उन विरोधाभासी बातों की गुत्थी को खोल दिया गया है। जैसे किसी चित्रकार की चेतना में अनंत चित्र एक ही साथ विद्यमान हो सकते हैं उसी प्रकार दिव्य परमात्मा में सभी भूतों का, सभी कुछ का आध्यात्मिक सह-अस्तित्व, सारूप्य और सहस्थिति है। सभी उनमें एक ही साथ अस्तित्वमान हैं और उन्हीं के स्वरूप के हैं। परंतु देश-काल से बद्ध होने के कारण हम देश-काल से परे किस प्रकार सभी चीजें सह-अस्तित्व में रह सकती हैं इसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते। जैसे कि, मानसिक स्तर पर भी हम समझ सकते हैं कि किसी कवि के मस्तिष्क में असंख्यों कविताएँ सह-अस्तित्व में हो सकती हैं, किसी चित्रकार के मस्तिष्क में अनेकानेक चित्र एक-साथ हो सकते हैं, परंतु जिसे इसका भान न हो वह तो यही सोचेगा कि सभी भिन्न-भिन्न कविताओं या चित्रों के लिए कवि या कलाकार के मस्तिष्क में भिन्न-भिन्न हिस्से बने हुए होंगे। परंतु मानसिक स्तर पर भी हम इस बात का बेतुकापन समझ सकते हैं क्योंकि हमें एक ऐसी मानसिक चेतना का अनुभव है जिसमें कि अनेकानेक चित्र या कविताएँ या अन्य रचनाएँ पूरी की पूरी एक साथ विद्यमान रह सकती हैं, उसी प्रकार दिव्य परमात्मा को चेतना में सभी कुछ का सहज रूप से आध्यात्मिक सह-अस्तित्व, सारूप्य और सहस्थिति है।
इसी को समझाने के लिए वर्तमान संदर्भ में आकाश-तत्त्व का उदाहरण दिया गया है। यदि हम आत्म-तत्त्व को आकाश-तत्व मानें तो उस आकाश तत्त्व के बिना तो किसी चीज का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। सारी ही चीजों का अस्तित्व आकाश के अन्दर होता है। पर उन चीजों में स्वयं में भी खाली जगह या फिर आकाश तत्त्व होता है। हमारे शरीर के अंदर और बाहर भी आकाश तत्त्व है, वैसे ही जैसे कि घट आकाश तत्त्व में है और उसके अंदर भी आकाश तत्त्व विद्यमान है। जब हम कहते हैं कि मनुष्य के अंदर परमात्मा व्याप्त हैं तो वे उसी तरह उसमें व्याप्त हैं जिस प्रकार घट में आकाश तत्त्व विद्यमान होता है। परंतु जिस प्रकार वह आकाश तत्त्व घट से सीमित नहीं हो जाता और सारे घट मिलकर भी आकाश तत्त्व को अपने में समाहित नहीं कर सकते उसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर व्याप्त होते हुए भी हमसे सर्वथा परे हैं। और जिस प्रकार घट से आकाश तत्त्व का निर्माण नहीं हो सकता, वह तो घट में व्याप्त होते हुए भी उससे एक स्वतंत्र तत्त्व होता है उसी प्रकार हममें व्याप्त होने पर भी परमात्म तत्त्व हमसे सर्वथा परे और स्वतंत्र होता है। इस प्रकार, घट और आकाश सर्वथा भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं। इसी उदाहरण को हम परमात्म तत्त्व और हमारे बीच लागू कर के समझ सकते हैं कि भले ही हम उस तत्त्व से बने हैं और उसी में निवास कर रहे हैं और हमारे अंदर वह तत्त्व विद्यमान है, तो भी वह तत्त्व हमसे सर्वथा भिन्न, स्वतंत्र और परे भी है। इसीलिए हम कितना भी ऊँचे से ऊँचा अनुमान क्यों न लगाएँ, तो भी उससे परमात्मा कभी सीमित नहीं हो जाते और न ही यह सृष्टि उन्हें पूर्ण रूप से कभी अभिव्यक्त ही कर सकती है। और चूंकि यह कभी पूर्ण रूप से उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर सकती इसी कारण यह उत्तरोत्तर विकसित होती रहती है, अधिकाधिक पूर्ण बनती रहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमात्मा को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया जा सके। पराप्रकृति अपनी पूरी सामर्थ्य लगाती है कि परमात्मा को अभिव्यक्त कर दे और इसके लिए वह असंख्यों ब्रह्माण्डों का निर्माण करती है, अनेकानेक स्तरों का सृजन करती है, नानाविध आयामों का निर्माण करती है तो भी परमात्मा उन सब में से बच निकलते हैं। इसी कारण हमें इस प्रकार की अद्भुत सृष्टि गोचर होती है जिसमें रूप तो सारे परमात्मा के ही हैं परंतु फिर भी परमात्मा उनसे सर्वथा परे हैं।
अब यदि हम परमात्मा की किसी ऐसे अनंत आयामी तत्त्व के रूप में परिकल्पना करें जिनके आयामों का कोई अंत नहीं है तो अभिव्यक्ति में तो वे किसी भी आयाम को मनचाहे क्रम से अभिव्यक्त कर सकते हैं और इस क्रम को हम काल की संज्ञा दे देते हैं जबकि अपने आप में तो उस तत्त्व में सभी आयाम साथ-साथ ही विद्यमान होते हैं। अतः देश और काल के अंदर शाश्वत के भिन्न-भिन्न गुण, भिन्न-भिन्न रूप अपने आप को प्रकट करते रहते हैं और जिसका जिस प्रकार का इंद्रिय-गठन होगा वैसा ही लोक उसके लिए प्रकट हो जाएगा। मनुष्यों की इंद्रियों से एक प्रकार को सृष्टि गोचर होती है, देवताओं, गंधर्वो, यक्षों आदि की भिन्न-भिन्त्र इंद्रियों से उनके अनुसार सृष्टि और लोक गोचर होते हैं, जबकि वास्तव में सभी एक ही तत्त्व को तो देख रहे होते हैं। यह तो वैसे ही है जैसे भगवान् श्रीरामचन्द्रजी को स्वयंवर के समय सब भिन्न-भिन्न भाव और रूप में देख रहे थे। जानकी जी उन्हें एक रूप में देख रही थीं, जनक जी दूसरे रूप में देख रहे थे, अन्य राजागण उन्हें बिल्कुल दूसरे ही रूप में देख रहे थे। अतः जिसकी जैसी भावना थी उसे वैसा ही रूप गोचर हो रहा था। इसी प्रकार परम सद्वस्तु 'एकमेवाद्वितीयम्' है और सभी उसी का दर्शन कर रहे हैं परंतु कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि स्वयं उसी का दर्शन ही पूर्ण है। सभी के दर्शनों को मिलाकर भी उस सद्वस्तु को पकड़ा नहीं जा सकता। यही बात भगवान् गीता में कह रहे हैं कि वे सब के अंदर स्थित भी हैं और किसी में भी स्थित नहीं है और सब कुछ से परे भी हैं। क्योंकि अपने आप में वह परमात्म तत्त्व तो सब कुछ से सर्वथा परे है और हम उस तत्त्व के क्या-क्या रूपक बनाते हैं उससे उसकी सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब निश्चेतन से लेकर अतिचेतन तक चेतना की अनंत श्रेणियाँ हैं और उन सब पर नानाविध अभिव्यक्तियाँ हैं और सभी दर्शन उन्हीं एक परमात्मा का ही करते हैं तो भी सभी दर्शनों में कितना अनंत वैविध्य हो गया है। साथ ही, जिस रूप का वे दर्शन करते हैं वह भी नित परिवर्तनशील, विकसनशील है जो कभी अपने आप को उसी रूप में पुनरावर्तित नहीं करता। इस प्रकार इस सब अनंत विविधता की तो हमारी चेतना में कल्पना करना भी संभव नहीं है।
अब इस विषय में एक अन्य आयाम का समावेश करते ही यह सारा परिदृश्य और भी जटिल बन जाता है। जिन अनंत श्रेणियों पर हम अनेकानेक अभिव्यक्तियों की बात कर रहे हैं वे सब परमात्मा स्वयं ही बने हैं और स्वयं ही अपना दर्शन या अवलोकन कर रहे हैं। इसीलिए हमारे वैदिक ऋषि कहते थे कि वास्तव में किसी चीज का सृजन नहीं होता। इसलिए वे इस सृष्टि को लोक कहते थे अर्थात् जैसा अवलोकन होगा वैसा ही हमें गोचर होगा। वही सृष्टि जिस रूप में किसी एक मनुष्य को गोचर होगी वैसी किसी कीट-पतंगे को नहीं होगी। और विभिन्न मनुष्यों को भी उनकी चेतना के अनुसार वह भिन्न-भिन्न गोचर होगी। साथ ही, किसी व्यक्ति-विशेष को भी उसकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न प्रतीत होगी। सांख्य इसका बड़े ही सटीक रूप से कारण बताता है कि क्यों हमें अपने मनोवैज्ञानिक गठन के अनुसार भिन्न-भिन्त्र चीज गोचर होती है। देवताओं का मनोवैज्ञानिक गठन भिन्न प्रकार का होने के कारण उन्हें जगत् भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। इसलिए, सभी केवल देखने के तरीके मात्र ही रह जाते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं।
भौतिक रूप से लगभग समान ही इंद्रियाँ होने पर भी प्रत्येक मनुष्य को एक भिन्न जगत् दिखाई देता है क्योंकि इंद्रियाँ मनस् को और मनस् बुद्धि को सूचना प्रदान करता है और वहीं से पूरे दृश्य का निर्माण होता है। यह चीज तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है जब हम किसी एक ही घटना का वृत्तांत दो विपरीत दृष्टिकोण के व्यक्तियों से सुनते हैं या किन्हीं दो बालकों की लड़ाई का ब्यौरा उनकी अपनी-अपनी माताओं के द्वारा सुनते हैं। अब भले दोनों ही माताओं की भौतिक इंद्रियाँ उन्हें लगभग समान ही सूचना देती हों परंतु उस सूचना का उनका मनस् और उनकी बुद्धि जो बना देते हैं वह तो बिल्कुल ही भिन्न होता है। हमारे चित्त में अनेकानेक वृत्तियाँ जमा होती हैं। पहले तो स्वयं के अनेक जन्मों की संचित वृत्तियाँ या संस्कार होते हैं, फिर अपने जातिगत, राष्ट्रगत आदि संस्कार भी होते हैं। हमारा जो भी निर्णय होता है उसमें इन सभी चीजों का हस्तक्षेप रहता है और इसी कारण सब का अपना-अपना जगत् होता है। इस सब चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि भले ही हमें इतने अनंतविध रूप दिखाई देते हों परंतु हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि इनमें से कोई एक ही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। ये सारे ही रूप परमात्मा के होने के बावजूद भी कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता और वे सदा इन सभी से सर्वथा परे रहते हैं। अब चूंकि परमात्मा किसी एक रूप से नहीं बंध जाते इसलिए भारतीय संस्कृति में पूजा-पद्धति के किसी भी रूप को कभी अस्वीकार नहीं किया गया। सभी को परमात्मा तक पहुँचने के संभव मार्गों के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है।
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ।। ७।।
७. हे कौन्तेय! कल्प के अन्त में समस्त भूत मेरी दिव्य प्रकृति में लौट जाते हैं; कल्प के आदि में उन्हें मैं फिर सृष्ट (उत्पन्न) कर देता हूँ।
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८॥
८. अपनी स्वयं की प्रकृति पर आश्रित होकर (उसे बाध्य करके), मैं अनेकानेक भूतों को, जो असहाय रूप से 'प्रकृति' के नियन्त्रण के वशीपुर हैं, बार-बार सृष्ट करता हूँ।
गीता में भगवान् ने भूतों को उत्पन्न करने की और स्वयं के जन्म ग्रहण की प्रणाली बताई है। चौथे अध्याय के छठे श्लोक में वे कहते हैं कि "यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, यद्यपि मैं अपनी आत्म-सत्ता में अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त भूतों का ईश्वर हूँ, तथापि मैं अपनी प्रकृति के ऊपर अधिष्ठित होकर अपनी माया के द्वारा जन्म ग्रहण करता हूँ।" अपनी टीका में इस भेद को स्पष्ट करते हुए श्रीअरविन्द ने चौथे अध्याय में कहा था कि, "अब यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा के एक हल्के से किन्तु फिर भी बड़े महत्त्वपूर्ण अंतर से गीता, समान ही रीति से, प्राणियों के सामान्य जन्म और एक अवतार के रूप में स्वयं के जन्म ग्रहण में भगवान् की क्रिया का वर्णन करती है। 'अपनी प्रकृति को वश में करके, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य,' और बाद में कहते हैं, 'मैं इन प्राणियों के समूह को जो प्रकृति के वश में हैं अवशं प्रकृतेर्वशात्, उत्पन्न करता हूँ, विसृजामि ।' और यहाँ कहते हैं कि, 'अपनी प्रकृति के ऊपर अधिष्ठित होकर मैं अपनी स्वयं की माया से जन्म लेता हूँ, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय आत्ममायया, मैं अपने-आपको उत्पन्न करता हूँ, आत्मानम् सृजामि।”
इसी दिव्य प्रकृति (प्रकृतिं मामिकाम्) की क्रिया में, भगवान् की निज प्रकृति (स्वां प्रकृतिम्) की क्रिया में जीव अपने भूतभाव के चक्र का अनुवर्तन करता है। उस प्रकृति के प्रगतिक्रम में होनेवाले दौरों या परिवर्तनों में जीव यह या वह व्यक्तित्व हो जाता है; उस दिव्य प्रकृति की एक अभिव्यक्ति के रूप में, चाहे उस प्रकृति की उच्चतर और प्रत्यक्ष गति में हो या उसकी निम्नतर और अप्रत्यक्ष गति में, चाहे अज्ञान में हो या ज्ञान में, जीव सदा ही अपने विशिष्ट स्वधर्म का पालन करता है; चक्र की गति पूरी होने पर प्रकृति अपनी प्रवृत्ति से निवृत्त होकर निश्चलता और निस्तब्धता को लौट जाती है। अज्ञान की दशा में प्रकृति के घूमते चक्रों के अधीन होता है, अपना स्वामी स्वयं नहीं होता अपितु प्रकृति के प्रभुत्व में रहता है, अवशः प्रकृतेर्वशात्, केवल दिव्य चेतना में सीटकर ही वह प्रभुता और मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ।। ९।।
९. और हे धनञ्जय! ये कर्म मुझे नहीं बाँधते क्योंकि इन कर्मों से अनासक्त हुआ मैं मानो उदासीनवत् इनके ऊपर स्थित हूँ।
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।। १०।।
१०. हे कौन्तेय! मेरी अध्यक्षता के अंतर्गत प्रकृति समस्त चराचर भूतों को उत्पन्न करती है; और इसके कारण जगत् आवर्तनों में चलता रहता है।
भगवान् भी प्रकृति के इस आवर्तन का पालन करते हैं, उसके अधीन होकर नहीं अपितु उसकी अंतर्व्याप्त आत्मा तथा मार्गदर्शक के रूप में, न उनकी सारी सत्ता इसमें सम्मिलित होती है, अपितु उनकी आत्मशक्ति प्रकृति का साथ देती और उसे आकार देती है। वे अपने ही प्रकृति-कर्म के अध्यक्ष होते हैं, - वे ऐसे जीव नहीं होते जो प्रकृति में जन्में हों अपितु वह सृजनशील आत्मा होते हैं जो प्रकृति से वह सब उत्पन्न करवाते हैं जो अभिव्यक्ति में नजर आता है। यदि अपनी आत्मशक्ति में वे प्रकृति के साथ-साथ होते हैं और उसकी सारी क्रियाएँ उससे कराते हैं, तो साथ ही वे उसके परे भी रहते हैं, मानो प्रकृति के सारे विश्वकर्म के ऊपर कोई अपने विश्वातीत प्रभुत्व में स्थित हो, किसी लिप्त करने वाली या वशीभूत करने वाली कामना के द्वारा वे प्रकृति से आसक्त नहीं हैं और इसलिए प्रकृति के कर्मों से बद्ध भी नहीं हैं, क्योंकि वे इन सब कर्मों से अनन्त रूप से परे हैं और उनसे श्रेष्ठ हैं, कालचक्रों में उनकी समस्त गति में उसके पहले, उसके मध्य में और अंत में वे समान ही रहते हैं। कालचक्रों के सभी परिवर्तनों से उनकी अक्षर सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मौन आत्मा विश्व को व्याप्त और धारण करती है वह वैश्विक परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती; क्योंकि, यद्यपि वह इन्हें धारण करती है पर इनमें भाग नहीं लेती। यह महत्तम परम विश्वातीत आत्मा भी प्रभावित नहीं होती क्योंकि वह इनको अतिक्रम किये है और शाश्वत रूप से इनके परे है।
इसमें यह अक्षर पुरुष के भाव का वर्णन है। परंतु क्षर भाव और अक्षर भाव दोनों ही का संचालन भगवान् की पराप्रकृति करती है जो स्वयं ही जीव की अंतरात्मा के रूप में आविर्भूत होती है जो निम्न प्रकृति और पराप्रकृति के बीच की कड़ी का काम करती है। इस प्रकार की व्यवस्था हमें गोचर होती है। इस जगत् का निर्माण दो पक्षों के समागम से ही होता है - एक है पुरुष पक्ष जो कि अवलोकन करता है और दूसरी है प्रकृति जिसका कि पुरुष साक्षित्व करता है। इन दो के बिना कोई भी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इनमें पुरुष तत्त्व को आत्म-तत्त्व का प्रतिनिधि कह सकते हैं और प्रकृति भगवान् की दिव्य प्रकृति की प्रतिनिधि है। इन दो के मिलन से ही कोई अभिव्यक्ति हो सकती है। यद्यपि हमारे इस सब वर्गीकरण से भगवान् बाध्य नहीं हो जाते, फिर भी इससे हमारी बुद्धि को कुछ सहारा मिल जाता है कि वह चीजों को कुछ अधिक समझ सके। अन्यथा भगवान् के विषय में तो निश्चयपूर्वक हम कह ही क्या सकते हैं।
परंतु इसके साथ ही, चूँकि यह कर्म भागवत् प्रकृति, स्वा प्रकृतिः, का कर्म है और भागवत् प्रकृति भगवान् से कभी पृथक् नहीं हो सकती, इसलिए जो कुछ भी वह सृष्टि करती है, भगवान् उसमें अवश्य अंतर्निहित होंगे। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जो भगवान् की सत्ता का संपूर्ण सत्य नहीं है, परंतु यह कोई ऐसा सत्य भी नहीं है जिसकी हम उपेक्षा कर सकते हों। वे मानव शरीर में बसे हैं। जो उनकी उस उपस्थिति को अनदेखा करते हैं, जो उसके बाहर मुखौटों के कारण मानवरूप में स्थित भगवत्ता की अवमानना करते हैं, वे प्रकृति की बाह्य प्रतीतियों के द्वारा भ्रमित और विमूढ़ होते हैं और वे यह अनुभव नहीं कर सकते कि हमारे अंदर गुप्त रूप से भगवान् स्थित हैं, चाहे वे मानवता में सचेतन हों जैसे कि एक अवतार में या फिर अपनी माया द्वारा प्रच्छन्न हों। जो महात्मा हैं, जो अपने अहं के भाव के अन्दर कैद नहीं हैं, जो अपने-आप को अंतर्यामी भगवान् के प्रति उद्घाटित करते हैं, वे जानते हैं कि मनुष्य में निहित गूढ़ आत्मा, जो यहाँ सीमित मानव-प्रकृति से बद्ध प्रतीत होती है, वह वही अनिर्वचनीय ज्योति या तेज है जिसे हम इस मानव रूप के परे परम परमेश्वर के रूप में पूजते हैं। वे भगवान् की उस परम स्थिति के बारे में सचेतन हो जाते हैं जिसमें वे सब भूतों के स्वामी और प्रभु हैं और फिर भी वे प्रत्येक भूत में देखते हैं कि वे ही प्रत्येक के परम देव और अंतःस्थित भगवान् भी हैं। बाकी जो कुछ है वह विश्व में प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों को अभिव्यक्त करने के लिए आत्म-परिसीमन है। वे यह भी देखते हैं कि यह उन्हीं भगवान् की प्रकृति है जो विश्व में जो कुछ भी है वह सब कुछ वही बनी हुई है, इसलिए यहाँ जो कुछ है, आंतरिक यथार्थता में और कुछ नहीं केवल वही एक भगवान् हैं, सब कुछ वासुदेव हैं, और वे उन्हें केवल विश्व के परे रहनेवाले परमेश्वर के रूप में ही नहीं पूजते अपितु यहाँ इस जगत् में, उनके एकात्म सत्वा अखण्ड रूप में तथा प्रत्येक पृथक् पृथक् जीव में भी पूजते हैं। वे इस सत्य को देखते हैं, और इसी सत्य में रहते और कर्म करते हैं; वे उन्हीं को सब पदार्थों के परे स्थित परम तत्त्व के रूप में तथा जगत् में स्थित ईश्वर के रूप में, और जो कुछ है उसके अधीश्वर के रूप में पूजते हैं, उन्हीं में निवास करते और उन्हीं की सेवा करते हैं, उनकी वे यज्ञकर्मों के द्वारा सेवा करते हैं, ज्ञान के द्वारा उनकी खोज करते हैं और उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं केवल उन्हें ही सर्वत्र देखते हैं और अपने जीवभाव में तथा अपनी बाह्य और आंतर प्रकृति में, दोनों ही प्रकार से अपनी सम्पूर्ण सत्ता को उन्हीं की ओर ऊपर उठाते हैं। इसे ही वे व्यापक, और बिल्कुल सही मार्ग मानते हैं; क्योंकि यही एकमेव परम तथा विश्वगत और व्यष्टिगत परमेश्वर के समग्र सत्य का मार्ग है।
महात्मा जन इसीलिए महात्मा कहे जाते हैं क्योंकि वे भगवान् के सत्स्वरूप को जानते हैं इसलिए भगवान् चाहे जिस किसी भी भेष में क्यों न आएँ, वे बाहरी आवरण से विमोहित हुए बिना उनके वास्तविक स्वरूप को कुछ हद तक पहचान जाते हैं। चूंकि उनका माया का पर्दा हट चुका होता है इसलिए उन्हें परमात्मा के अचिंत्य रूप का भी आभास होता है और साथ ही हर छोटे से छोटे प्राणी में, यहाँ तक कि भौतिक पदार्थों में भी उन्हें प्रकट रूप में यह दिखाई देता है कि परमात्मा स्वयं ही उन सब रूपों में प्रकट हो रहे हैं इसलिए उन रूपों को वे अनदेखा नहीं करते और न ही वे उन रूपों के आवरण से भ्रमित ही होते हैं जो प्रभु ने स्वयं के ऊपर डाल रखा है क्योंकि उस आवरण के पीछे वे उन परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं और न केवल वे उनका दर्शन ही करते हैं अपितु उनसे प्रेम भी करते हैं। और जो कोई चेतना की इस अवस्था में होगा वह तो 'सर्वभूतहितेरताः' सभी भूतों के हित में रत रहेगा ही, इसके अतिरिक्त तो वह और कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिये छठे अध्याय के इकतीसवें श्लोक में भगवान् कहते हैं कि जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर समस्त भूतों में मुझसे प्रेम करता है वह योगी चाहे जिस प्रकार रहे और कर्म करे मुझमें ही रहता और कर्म करता है। इस प्रकार यहाँ महात्माओं और ऋषियों की स्थिति का वर्णन है। वे परमात्मा का उनके सत्स्वरूप में भी दर्शन करते हैं और इस प्रकृति के अंदर जो अभिव्यक्त रूप उन्होंने धारण किये हैं उनमें भी वे उन्हीं परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। वास्तव में तो परमात्मा स्वयं को ही तो देख रहे हैं क्योंकि उनके अतिरिक्त तो अन्य कोई सत्ता है ही नहीं। वे स्वयं ही प्रकृति हैं और स्वयं ही पुरुष हैं जो स्वयं का ही साक्षित्व करते हैं। परंतु हमारा जिस प्रकार का ताना-बाना बना हुआ है उसमें हमारी इंद्रियाँ हमें इतने सारे रूप दिखाती हैं और उन रूपों के पीछे के एकत्व को, उन परमात्मा को चूक जाती हैं। परंतु महात्मा जन अपनी इन इंद्रिय सीमाओं को तोड़कर बाह्य प्रतीतियों के पीछे प्रभु की झलक पा लेते हैं। वे अपने परम् प्रिय को सर्वत्र देखते हैं इसलिए उन्हें कोई भय नहीं रहता।
vi.31
गीता वर्तमान प्रसंग में जिस चीज का वर्णन कर रही है वह कोई केवल एक दार्शनिक या तत्त्वसंबंधी बात ही नहीं अपितु भावात्मक बात भी है। इससे तो सारे जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। गीता इन्हीं भावात्मक तत्त्वों का अधिकाधिक निरूपण करती जाएगी क्योंकि अब वह भक्तियोग की ओर मुड़ती जा रही है। पहले छः अध्यायों में कर्म और ज्ञान का समन्वय और उसके बाद सातवें अध्याय में ज्ञान और भक्ति का समन्वय साधने के बाद अब आगे गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का समन्वय साधने की ओर अग्रसर हो रही है। भगवान् कहते हैं कि जो कर्म उनके लिए और उनकी भक्ति के रूप में किये जाते हैं वे ही सच्चे कर्म हैं बाकी सारे तो अकर्म हैं। जब व्यक्ति अपने आप को पृथक् समझकर अहमात्मक चेतना से कर्म करता है तब वह कर्म न करके अकर्म ही करता है। कर्मयोग तो केवल वही है जो प्रभु से प्रेम के कारण किया जाता है। हमारे श्रीअरविन्द आश्रम का आधार ही यही है कि श्रीमाताजी से प्रेम के वशीभूत हो कार्य करना।
अतः, यही पूर्ण सत्य, उच्चतम और विस्तृततम ज्ञान है। भगवान् विश्वातीत हैं, सनातन परब्रह्म हैं, जो अपनी देशकालातीत सत्ता से, अपनी स्वयं को सत्ता और प्रकृति से इस सारी वैश्विक अभिव्यक्ति को देश और काल के अन्दर धारण करते हैं। वे ही वे परमात्मन् हैं जो जगत् के रूपों और गतियों को अंतरीय आत्मा हैं। वे ही पुरुषोत्तम हैं जिनका कि सब जीवात्मा और प्रकृति, सारा आत्मभाव और इस जगत् का या किसी भी जगत् का सारा भूतभाव आत्म-संकल्पन (self-conception) और आत्म-स्फूर्तिकरण (self- energising) है। वे ही सब भूतों के अनिर्वचनीय परमेश्वर हैं, जो प्रकृति में आविर्भूत हुई निज शक्ति को अपने आत्मिक नियंत्रण के द्वारा जगत् के चक्रों और उन चक्रों में प्राणियों के प्राकृत विकास में उद्घाटित करते रहते हैं। जीव. व्यष्टि पुरुष, प्रकृतिस्थ आत्मा, उन्हीं की सत्ता से अस्तित्वमान है, उन्हीं की चेतना के प्रकाश से सचेतन है, उन्हीं के संकल्प और शक्ति से जिसमें ज्ञान-शक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति है, उन्हीं के दिव्य विश्वभोग से जो अस्तित्व का भोग करता है, और उन्हीं से इन विश्वचक्रों में आया है।
परमात्मा के ये चार रूप हैं : परंब्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम, परमेश्वर। हालाँकि ये सब हैं एक ही परंतु चार भिन्न क्रियाओं के अनुसार देखने के कारण हम उन्हें चार नाम दे देते हैं। जब उन्हें आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो वे परमात्मा हैं। जब सर्वस्थित ब्रह्म के रूप में जगत् की व्याख्या करें तो वे परंब्रह्म हैं। सबके नियंता ईश्वर के रूप में देखें तो वे परमेश्वर हैं और यदि सब कुछ का साक्षित्व करने वाले पुरुष के रूप में जगत् की व्याख्या करें तो वे पुरुषोत्तम हैं। इन्हीं की ओर समग्र रूप से चलने के लिए अब कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय को साधने का सूत्र दिया जा रहा है।
II. कर्म, भक्ति और ज्ञान
मनुष्य की अंतरात्मा यहाँ भगवान् का ही आंशिक आत्मप्राकट्य है, जो जगत् में भगवान् की प्रकृति के कर्मों के लिये स्वतः-सीमित हुई है, प्रकृतिर्जीवभूता। अपने आत्मतत्त्व में व्यक्ति भगवान् के साथ एक है।... प्रकृति की निम्नतर बाह्य-प्रतीति में एक प्रकार के अज्ञान और अहंकारमय पार्थक्य के कारण यह जीव 'एकमेव' से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है और इस पृथकात्मक चेतना में रहते हुए अपने अहंपरक सुख-भोग और जगत् में अपने व्यक्तिगत अस्तित्व और अन्य देहधारी मनों और प्राणों के साथ अपने बाह्य संबंधों की प्रयोजनसिद्धि के लिए ही चिंतन, इच्छा, कर्म करता और उसी में सुख-भोग लेता प्रतीत होता है। परन्तु वास्तव में उसकी सारी सत्ता, उसका सारा चिंतन, उसकी सारी इच्छा, कर्म और भोग भगवान् की सत्ता, भगवान् के विचार, संकल्प, कर्म और प्रकृति के भोग का ही एक प्रतिबिम्ब मात्र होता है - ऐसा प्रतिबिम्ब जो तब तक अहंकारमय और विकृत ही रहता है जब तक जीव अज्ञान में रहता है। अपने-आप के इस सत्य पर लौटना, इसे पुनः प्राप्त कर लेना ही उसकी मुक्ति का सीधा साधन है, अज्ञान की दासता से छूट निकलने का उसके लिए यही सबसे विशालतम और निकटतम द्वार है। चूँकि वह एक आत्मा है, एक ऐसी अंतरात्मा जो मन और तर्कशक्ति की, इच्छाशक्ति और ऊर्जस्वी कर्म की, भावना और संवेदना की तथा अस्तित्व का आनन्द पाने की प्राण की कामना की प्रवृत्ति से युक्त है, अतः इन्हीं सब शक्तियों को भगवन्मुखी कर देने से उसके लिए अपने परम सत्य पर पुनः लौटना पूर्णतया संभव हो सकता है। उसे परमात्मा और ब्रह्म के ज्ञान से जानना होगा; उसे अपनी प्रेम-भक्ति और आराधना परम् पुरुष की ओर मोड़ देनी होगी; उसे अपने संकल्प और कर्मों को परम जगदीश्वर के अधीन करना होगा। तब वह निम्न प्रकृति से दिव्य प्रकृति की ओर अग्रसर होता है…
vii-5
प्रश्न : मन और प्राण के बाह्य संपकों और संबंधों को किस प्रकार त्यागा जाए जिनमें कि हम सब समय लिप्त रहते हैं और जिसके कारण हम वास्तविक चीज को अनदेखा कर देते हैं?
उत्तर : इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता अपितु दूसरी दिशा में मोड़ना पड़ता है। कर्मप्रधान व्यक्ति अपने कर्मों को अधिकाधिक भगवान् के निमित्त करने का प्रयास करता है। ज्ञानमार्गी ध्यान-चिंतन, ब्रह्म की कल्पना, धारणा, तत्त्वचिंतन आदि अनेकानेक पद्धतियों का सहारा लेकर उन्हीं में लीन होने का प्रयास करता है और उस ओर अपनी सारी वृत्तियों को मोड़ने का प्रयास करता है। भावप्रधान व्यक्ति अपने भावों को उस ओर मोड़ने का प्रयास करता है। अपने गठन के अनुसार व्यक्ति किसी भी एक के सहारे अपनी गतियों को उस ओर मोड़ने का प्रयास करता है और धीरे-धीरे अन्य हिस्सों पर उसका प्रभाव फैलता जाता है जिससे कि अन्य हिस्से भी उस ओर मुड़ने लगते हैं। गीता सभी भागों को भगवान् की ओर मोड़ने की माँग करती है। गीता ने अपनी शिक्षा का आरंभ कर्मों को भगवन्मुख करने से किया और कर्मयोग का निरूपण किया। कर्म का निरूपण करते-करते गीता उसमें यह कहते हुए ज्ञान का समावेश करती है कि ज्ञान कर्मों से श्रेष्ठ है और उसी के द्वारा सच्चे कर्म किये जा सकते हैं। इस प्रकार गीता कर्म और ज्ञान का समन्वय साधती है। इनका निरूपण करते-करते वह इस बिन्दु तक पहुँचती है कि ज्ञानियों में भी जो भगवान् का भक्त है वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ज्ञान और कर्म में एक नए तत्त्व - भक्ति - का समावेश कर वह इन तीनों का समन्वय साधती है। मन की प्रवृत्ति है ज्ञान अर्जित करने की, इच्छा शक्ति की प्रवृत्ति है कुछ संसिद्ध करने की, अपने आप को परिपुष्ट करने की, और भावात्मक पक्ष की प्रवृत्ति है भावना के द्वारा आनंद प्राप्त करने की। पर इन सभी भागों में प्राण का प्रवेश होता है और वह इन सभी के माध्यम से सुख बटोरने की कोशिश करता है। आरंभ में जब व्यक्ति कुछ आस्तिक होता है और अपने से अतिरिक्त किसी उच्चतर विधान या किसी उच्चतर सत्ता को स्वीकार करता है तब वह अपने सुख की पुष्टि के लिए उसकी सहायता लेने के लिए उसकी ओर मुड़ता है। उसकी ओर मुड़ने में उसके अनेक हेतु हो सकते हैं। या तो वह अपने किसी संकट या समस्या के समाधान के लिए, अपने किसी हेतु या उद्देश्य की पूर्ति या सिद्धि के लिए या फिर किसी प्रकार की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसकी ओर मुड़ सकता है। आरंभ में इन किन्हीं भी हेतुओं से व्यक्ति भगवान् की ओर मुड़ता है और इस प्रकार यह आदान-प्रदान आरंभ हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति को यह अनुभव नहीं हो जाता कि भगवान् केवल किसी स्वार्थ सिद्धि हेतु ही निकट जाने योग्य नहीं हैं अपितु उनकी स्वयं की चाह रखना और उन्हें प्राप्त करना तो इन सब निम्न हेतुओं से अनंततः श्रेष्ठ, आनंददायक और तुष्टिप्रद है। इस प्रकार यह एक विकासक्रम है जिसमें आरंभ में व्यक्ति अपने अहं के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता और केवल अपने पुरुषार्थ को ही अपने अहं की तुष्टि का एकमात्र साधन मानता है। उस अवस्था से कुछ विकसित होकर वह कुछ आस्तिक बनता है और अपने पुरुषार्थ के साथ ही साथ किसी अन्य विधान और सत्ता को भी स्वीकार करने लगता है और अपनी तुष्टि के लिए उसकी सहायता की पुकार करता है। धीरे-धीरे जब उसका आदान प्रदान उस सत्ता के साथ, भगवान् के साथ बढ़ता है तब वह उनके स्वरूप के विषय में कुछ अधिक सज्ञान होता है। और तब वह उनसे सुख खोजने की बजाय उन्हीं की सत्ता में आनंद लेने लगता है। उसे अपने सभी भागों की परिपूर्ति उन्हीं में अनुभव होने लगती है और वह यह जान जाता है कि सभी सुखों के मूलस्रोत केवल वे ही हैं इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किन्हीं भी परोक्ष साधनों के माध्यम से सुख खोजने की चेष्टा करने की बजाय जो सच्चे आनंद के निधान हैं उन्हीं के पास जाया जाए, उन्हीं की सत्ता में गोता लगाया जाए। इसे ही सत्ता का समग्र रूप से भगवान् की ओर मुड़ना कहते हैं। परंतु यह समग्र मुड़ाव आरंभ में ही संभव नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर अनेकानेक ऐसे भाग होते हैं जिनके अपने-अपने निहित निम्न उद्देश्य होते हैं और वे उन्हीं को पूरा करने की चेष्टा करते रहते हैं। परंतु यदि एक बार व्यक्ति में यह संकल्प आ जाए कि सब कुछ के बावजूद उसे अपने आप को भगवान् की ओर मोड़ना है तब फिर धीरे-धीरे आरोहण का मार्ग खुल जाता है। अतः एक बार जब व्यक्ति को भगवान् की सत्ता का कुछ स्पर्श प्राप्त हो जाए, उनका कुछ आस्वादन प्राप्त हो जाए तब फिर वह अधिकाधिक उन्हीं की ओर अपने सभी भागों को मोड़ने का प्रयास करने लगता है क्योंकि उनके अंदर उसे जो सुख, शांति, प्रकाश, प्रेम, आनंद, परिपूर्ति आदि प्राप्त होते हैं वे तो अन्य कहीं किसी चीज से उसे प्राप्त ही नहीं होते। परंतु इस अवस्था के बाद भी एक अवस्था है जहाँ व्यक्ति भगवान् में आनंद खोजने की बजाय उन्हीं का हो जाना चाहता है और अपनी संपूर्ण सत्ता को उन्हीं को समर्पित कर देता है ताकि वे उसका अपने संकल्प की अभिव्यक्ति के लिए जैसा चाहे वैसा उपयोग करें। यही पराभक्ति है। इसलिए जब कहते हैं कि 'योग भगवान् के हित किया जाता है' तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हमें भगवान् प्राप्त हो जाएँ, अपितु यह होता है कि हम पूर्ण रूप से भगवान् के हो जाएँ और वे हमारी सत्ता का उपभोग करें। पराभक्ति में तो इतना शुद्ध भाव होता है कि वह अपनी निजी तुष्टि के विषय में तो कुछ सोच ही नहीं सकती। उसका भाव तो एकमात्र यह होता है कि उसके प्रेमास्पद उसका उपभोग करें और उसी में उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार ये सभी आरोहण की विभिन्न अवस्थाएँ हैं। परंतु वर्तमान में गीता हमारे सभी भागों को भगवान् की ओर मोड़ने की माँग करती है क्योंकि इसी मुड़ाव के द्वारा अज्ञान से मुक्ति हो सकती है।
जीव का भगवान् की ओर इस प्रकार सर्वभाव से मुड़ना ही गीता के ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय को शानदार ढंग से स्थापित करता है। इस प्रकार भगवान् को सर्वभावेन जानना उन्हें इस रूप में जानना है कि वे हो 'एकमेव भगवान्' आत्मा में हैं, समस्त अभिव्यक्ति में हैं और समस्त अभिव्यक्ति के परे हैं, - और यह सब वे एक ही साथ और एक ही समय में हैं। परन्तु फिर भी, उन्हें इस प्रकार जानना भी पर्याप्त नहीं होता जब तक कि उसके साथ-ही-साथ हृदय और अंतःकरण का तीव्र रूप से भगवन्मुख उत्थान न हो जब तक कि वह एकनिष्ठ और साथ-ही-साथ सर्वसमावेशी प्रेम, भक्ति और अभीप्सा को प्रज्ज्वलित न कर दे। निश्चय ही वह ज्ञान जो किसी अभीप्सा से युक्त न हो, जो किसी उन्नयन से अनुप्राणित नहीं होता, वह कोई सच्चा ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह तो केवल बौद्धिक रूप से देखने की क्रिया और व्यर्थ ज्ञान-संबंधी प्रयास मात्र ही हो सकता है। भगवान् का दर्शन अनिवार्य रूप से भगवान की भक्ति और उन्हें ढूँढ़ने की सच्ची लगन ले आता है, - अपने स्वयं-सिद्ध स्वरूप में ही भगवान् के लिए लगन नहीं अपितु उन भगवान् के लिए भी जो हमारे अन्दर हैं और उन भगवान् के लिए भी जो कि जो कुछ भी है उस सबके अन्दर हैं। बुद्धि से जानना केवल समझना है और यह एक कारगर आरंभ-बिंदु हो सकता है, - पर साथ ही, हो सकता है ऐसा न हो. और अवश्य ही ऐसा नहीं होगा यदि उस ज्ञान में कोई सच्चाई न हो, संकल्प में इसकी आंतरिक अनुभूति के लिए कोई उत्कण्ठा न हो, अंतर्भाव में कोई शति न हो, आत्मा के अन्दर कोई पुकार न होः क्योंकि तब उसका अर्थ होगा कि मस्तिष्क ने केवल बाहरी रूप से ही समझा है, परंतु आंतरिक रूप से आत्मा ने कुछ नहीं देखा है। वास्तव में यदि हम अपनी स्थिति देखें तो हम पाएँगे कि हम अधिकांशतः अपने कामपुरुष की तुष्टियों में ही लगे रहते हैं और चूंकि उसी भाग को अधिकांश पोषण मिलता है इसलिए वही हृष्ट-पुष्ट होता है जबकि दूसरे भाग कुपोषित और तिरस्कृत रहते हैं। इसलिए यदि मस्तिष्क, बुद्धि आदि भागों में छोटा-मोटा ज्ञान हो भी तो वह कामनाओं आदि के नीचे दबे होने के कारण प्रभावी नहीं होता। उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वह जीवन पर कोई प्रभाव डाल सके, हमारे कर्मों को संचालित कर सके। इसलिए भले ही बुद्धि में किसी प्रकार का कोई क्षीण आदर्श या ज्ञान हो तो भी हमारे कर्म तो केवल प्राणिक इच्छाओं-कामनाओं की सेवा में ही लगे रहते हैं। हमारी आत्मा को पोषण तो तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति परमात्मा की ओर अभिमुख हो तथा उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करे। हमारे हृदय की गहरी अभीप्सा को अभिव्यक्ति का जितना ही अधिक अवसर प्राप्त होगा उतना ही पोषण हमारी अंतरात्मा को मिलेगा और वह सुदृढ़ होती जाएगी। वर्तमान में तो अधिकांशतः कामपुरुष को ही अपनी अभिव्यक्ति का मौका मिल रहा है। पूरे विश्व में केवल इसी की तुष्टि पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान सभ्यता तो प्रधानतः इसी पर केंद्रित है कि किस प्रकार अधिकाधिक प्राणिक सुख-भोग की पूर्ति हो सके। हमारी सारी व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ, शिक्षा आदि लगभग सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एकमात्र इसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन जुटाने में लगी हैं। सामान्यतः हमारी तथाकथित ऊँची से ऊँची चीजें भी केवल एक भिन्न रंग-रूप में इसी की पूर्ति में लगी हैं। और चूंकि हम चेतना की एक ऐसी अवस्था में रहते हैं जहाँ हमें केवल सुख-भोग की तुष्टि ही नजर आती है, इसलिए कोई भी गंभीर ज्ञान, अंतर्बोध, गहरी अभीप्सा आदि हमसे दूर रहते हैं और हमें उनका जरा भी स्वाद प्राप्त नहीं होता।
अंतःसत्ता से जानना ही सच्चा ज्ञान है, और जब अंतःसत्ता प्रकाश द्वारा स्पर्श की जाती है तब जिस चीज को उसने देखा है उसे आलिंगन करने, ग्रहण करने के लिए वह उठ खड़ी होती है, उसे अधिकृत करने के लिए वह लालायित हो उठती है, उसे अपने अन्दर और अपने-आप को उसके अन्दर रूपान्वित करने के लिए अथक प्रयास करती है, उसने जो दर्शन किया है उसके वैभव के साथ एक होने के लिए परिश्रम करती है। इस अर्थ में ज्ञान अभिन्नता या तादात्म्य की ओर जागृति है, और चूँकि अंतःसत्ता चेतना और आनन्द के द्वारा, प्रेम के द्वारा, निजस्वरूप का जो कुछ दर्शन उसे हुआ है उसकी प्रि और उसके साथ एकत्व के द्वारा आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करती है, इसलि ज्ञान जागृत होने पर अवश्य ही इस सच्चे और एकमात्र पूर्ण साक्षात्कार की दिशा में एक सर्वातिशयी अंतःप्रेरणा ले आता है। यहाँ जिस तत्त्व का ज्ञा होता है, वह कोई बाह्य विषय नहीं, अपितु दिव्य पुरुष का, हम जो कुछ भी। उसकी आत्मा और प्रभु का ज्ञान होता है। उनमें एक सर्वग्राही आनंद औ उनके प्रति एक गंभीर और द्रवित प्रेम और भक्ति ही इस ज्ञान का अवश्यंभाने परिणाम और इसकी स्वयं आत्मा ही है। और यह भक्ति हृदय की ही कोर एकांगी खोज नहीं, अपितु संपूर्ण सत्ता का ही अर्पण है। इसलिए अवश्य है यह एक यज्ञ का रूप भी ले लेगा; क्योंकि इसमें हमारे सभी कर्मों का ईश्वर के प्रति दान होता है, हमारी सारी सक्रिय अंतर्बाह्य प्रकृति का उसकी प्रत्येक आत्मनिष्ठ और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ क्रिया में अपने प्रिय भगवान् के प्रति समर्पण होता है। हमारी समस्त आत्मनिष्ठ क्रियाएँ उन्हीं में गति करती हैं और उन्हों प्रभु और आत्मा को अपनी शक्ति और प्रयास के मूलस्रोत और लक्ष्य के रूप में खोजती हैं। हमारी समस्त बाह्य अथवा वस्तुनिष्ठ क्रियाएँ जगत् में उन्हीं की ओर गतिमान होती हैं और उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाती हैं, भगवत्सेवा के कार्य का ऐसे जगत् में आरंभ कराती हैं जिसकी नियामक शक्ति हमारे वे अंतःस्थ भगवान् हैं जिनके अन्दर हम जगत् और उसके प्राणियों के साथ एकात्मा हैं। क्योंकि, जगत् और आत्मा, प्रकृति और प्रकृतिस्थ पुरुष दोनों उसी 'एक' की चेतना से प्रकाशमान हैं और दोनों ही उन्हीं परात्पर पुरुषोत्तम के हो आन्तर और बाह्य विग्रह हैं। इस प्रकार एकमेव आत्मा और आत्मभाव के अन्दर बुद्धि, हृदय और संकल्प का समन्वय साधित होता है और इसके साथ इस पूर्ण मिलन में, इस सर्वसमावेशी भगवत्साक्षात्कार में, इस दिव्य योग में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय साधित होता है।
परन्तु इस स्थिति तक किंचित्मात्र भी पहुँचना अहंबद्ध प्रकृति के लिये कठिन है। और इस स्थिति की विजयी और समस्वर पूर्णता पर पहुँचना तो तब भी सुगम नहीं होता जब हमने अन्ततः और सदा के लिए इस मार्ग पर कदम रख दिये होते हैं।
प्रश्न : क्या हम कह सकते हैं कि भक्ति का स्रोत ज्ञान है?
उत्तर : भक्ति का स्रोत ज्ञान नहीं है। हम कह सकते हैं कि ज्ञान आने से भक्ति के मार्ग का रोड़ा हटता है अन्यथा तो ज्ञान अपने आप में अधूरा रहता है जो कि भक्ति के मार्ग में बाधक होता है। जब सच्चा ज्ञान आ जाता है तब वह भक्ति के मार्ग में बाधक नहीं अपितु सहायक हो जाता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्ति का स्रोत ज्ञान है। अपने आप में भक्ति ही है जो ज्ञान और कर्म को अपने साथ समन्वित कर सकती है। ज्ञान का सामान्यतया जो अर्थ लगाया जाता है वास्तव में वह ज्ञान नहीं है। सामान्यतया ज्ञान से हम अर्थ लगाते हैं कि प्रकृति-पुरुष के भेद का पता लग जाना, ब्रह्म के विषय में कुछ पता लग जाना, संसार माया का खेल नजर आना, आदि-आदि। परंतु इसी अध्याय के तीसवें श्लोक में स्वयं गीता ही कहती है कि यदि बहुत दुराचारी मनुष्य भी अनन्य और पूर्ण प्रेम के साथ भगवान् की ओर मुड़ता है तो वह साधु मानने योग्य है। अतः, जिसके यह समझ में आ गया कि संसार में परमात्मा ही एकमात्र वरण करने योग्य हैं, वही सच्चा ज्ञानी है बाकी सब तो केवल व्यर्थ की चेष्टाएँ या प्रयास मात्र ही हैं। उदाहरण के लिए, भले ही कोई व्यक्ति किसी अमुक व्यक्ति से पहली बार ही मिला हो और उसके विषय में कुछ भी न जानता हो परंतु फिर भी उसे अंदर से यह महसूस हो सकता है कि वही व्यक्ति उसका आराध्य है, उसी की सेवा करना उसके संपूर्ण जीवन का लक्ष्य है, उसी के चरणों में वह अपना सर्वस्व अर्पित कर सकता है। भले ही अनेकों लोग उस व्यक्ति के पास जाते हों और उसके प्रति मन में बड़ा आदर भाव भी रखते हों परंतु कोई सच्चा शिष्य ही है जो उसे तत्क्षण पहचान जाएगा और उसके प्रति आत्मसमर्पण के द्वारा भगवान् को प्राप्त कर लेगा जबकि दूसरों को उसी व्यक्ति के सान्निध्य से संभवतः कुछ भी प्राप्त न हो। यह पहचान ही सच्चा ज्ञान है। यही सच्ची समझ है। यह एक बिल्कुल भिन्न गति है, भिन्न भाव है। व्यक्ति तब यह नहीं सोचता कि अब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है इसलिए उसे परमात्मा की ओर चलना चाहिये। सच्चे ज्ञान का तो अर्थ ही यही है कि व्यक्ति अनायास ही परमात्मा की ओर चल पड़ता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि परमात्मा की इस यात्रा में मार्ग निष्कंटक होगा। जो भी इस मार्ग पर गए हैं वे सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मार्ग अत्यंत कठिन मार्ग है जिस पर कदम-कदम पर धोखे हैं, जाल-घात हैं। परंतु फिर भी जिसे एक बार भी भीतर से सच्चा संस्पर्श प्राप्त हो गया है वह तो कितनी भी तकलीफों के बावजूद भी उस मार्ग पर आगे बढ़े बिना नहीं रह सकता। सच्चे ज्ञान में निश्चयात्मकता होती है। गोपियों को सच्चा ज्ञान था इसीलिए उद्धव की सारी ज्ञान सरीखी बातों का उन पर जरा भी प्रभाव नहीं हुआ। सभी सच्चे आध्यात्मिक महापुरुषों के जीवन में हम यह बात देख सकते हैं कि उनकी निष्ठा अनन्य होती है और वे अपने इष्ट के प्रति बड़े निश्चयात्मक होते हैं, इस विषय में उनमें कोई भ्रम नहीं होता। आंतरिक ज्ञान और अनुभव निश्चयात्मकता लाते हैं। यदि ऐसा न होता तो किस प्रकार या किस आधार पर एक क्षण में ही व्यक्ति अपना सर्वस्व किसी पूजा के पात्र पर सहर्ष न्यौछावर कर सकता था। इस निश्चयात्मकता के अभाव में ही तो बहुत से व्यक्ति जीवन भर यह तय नहीं कर पाते कि वास्तव में करना क्या चाहिये और इसी भ्रमपूर्ण स्थिति में जीवन बीत जाता है। परंतु ज्यों ही व्यक्ति को भीतरी स्पर्श प्राप्त होता है त्यों ही निश्चयात्मकता आ जाती है कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। इस अनुभव को हम केवल मानसिक रूप से कभी भी नहीं समझ सकते।
-------------------------------------
* उनकी सत्ता मन के परे का एक रहस्य है,
उसके तौर-तरीके मर्त्य अज्ञानता को चकरा देते हैं;
सीमित' अपने नन्हें विभागों में स्थित,
चकित, भगवान् के सामर्थ्य को श्रेय नहीं देता
जो अकल्पित 'सर्वं' बनने का साहस करता है,
और एक अनन्त की भाँति सदा देखता और कार्य करता है।
मानव के तर्क के विरुद्ध उनका यह अपराध है,
ज्ञात होकर भी नित्य अज्ञेय बने रहना,
सब कुछ होकर भी फिर इस गुह्य समग्रता को लाँघ जाना,
'निरपेक्ष' होकर 'काल' के एक सापेक्ष जगत् में निवास करना,
शाश्वत और सर्वज्ञ होकर जन्म का कष्ट उठाना,
सर्वशक्तिशाली होकर 'दैवयोग' और 'नियति' से खेल करना,
'आत्मा' होकर भी जड़ और शून्य बनना,
असीम, नामरूपातीत होकर,
एक देह में निवास करना, एकमेव और परम होकर
पशु एवं मानव एवं देव बनना…
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ।। ११ ।।
११. मूढ़ मनुष्य मुझे मानव देह में आश्रित या आवासित जानकर मेरी उपेक्षा करते हैं क्योंकि वे मेरे समस्त भूतों के ईश्वर स्वरूप, मेरे परं भाव ३, को नहीं जानते।
मर्त्य मन आवरणों और बाह्य प्रतीतियों पर अपने अज्ञ भरोसे के कारण संभ्रमित हो जाता है; वह केवल बाह्य मानव शरीर, मानव मन, मानव जीवनचर्या ही देखता है और उन भगवान् की कोई मुक्तिदायी झलक नहीं पकड़ पाता जो प्राणी में निवास करते हैं। वह स्वयं अपने अन्दर के भगवत्तत्व की उपेक्षा कर देता है और दूसरे मनुष्यों में भी उसे नहीं देख पाता, और तब भी जब मानवजाति के अंदर भगवान् अपने-आप को अवतार और विभूति के रूप में प्रकट करते हैं, वह फिर भी अंधा ही बना रहता है और प्रच्छन्न भगवान् की उपेक्षा या अवहेलना करता है, अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। और, जब वह जीवित प्राणी के अन्दर उनकी उपेक्षा करता है तब उस बाह्य जगत् में तो वह उन्हें देख ही क्या सकता है जिसे वह अपने पृथक्कारी अहंकार की कैद के कारण सीमित मन-बुद्धि के बन्द झरोखों से झाँकता है। वह ईश्वर को जगत् में नहीं देखता; उन परमेश्वर के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता जो इन विविध भूतों से परिपूर्ण लोकों के स्वामी हैं और उन भूतों में निवास करते हैं; वह उस दृष्टि के प्रति अंधा है जिसके द्वारा संसार में सभी कुछ दिव्य हो उठता है और जीव स्वयं अपने अंतर्निहित भगवान् के प्रति जाग उठता है और भगवान् का हो जाता है, भगवत्सदृश हो जाता है।
मोघाशा मोषकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ।। १२।।
१२. वे व्यर्थ की आशाओं, व्यर्थ कर्मों और व्यर्थ ज्ञान वाले होते हैं। सच्ची चेतना से शून्य वे भ्रमित करने वाली राक्षसी और आसुरिक प्रकृति में निवास करते हैं।
जिन लोगों ने सीमित चीजों के लिए और बुद्धि, देह व इंद्रियों की पार्थिव लालसा की तुष्टि के लिए स्वयं को अतिशय पूर्ण रूप से अहंमय जीवन में झोंक दिया है... वे निम्न प्रकृति के हाथों में जा गिरते हैं... वे लोग मनुष्य के अन्दर उस राक्षस की प्रकृति के शिकार हो जाते हैं जो अपने पृथक् प्राणमय अहंकार की उग्र और अदम्य भोग-लालसा पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है और उस (प्राणमय अहंकार) को ही अपनी इच्छा, चिंतन, कर्म और भोग का अंधकारमय देव बना लेता है। अथवा वे आसुरी प्रकृति की अहंकारी स्वेच्छा, स्वतःसंतुष्ट विचार, स्वार्थांध कर्म, स्वतः-संतुष्ट पर फिर भी सदा असंतुष्ट रहनेवाली बौद्धिकभावापन्न भोग-तृष्णा के द्वारा व्यर्थ के चक्कर में घसीट लिए जाते हैं। परन्तु दुराग्रहपूर्वक सदा इस पृथक्कारी अहं-चेतना में जीना और उसे ही अपने सारे क्रियाकलापों का केन्द्र बना लेना अपने सच्चे आत्म-बोध से सर्वथा वंचित हो जाना है। जो मोह-जाल यह आत्मा के पथभ्रष्ट उपकरणों पर डालता है वह एक ऐसा सम्मोहन है जो जीवन को एक फलहीन चक्कर से बाँध देता है। भगवदीय और सनातन मापदण्ड से आँकलन करने पर उसकी समस्त आशा, कर्म, ज्ञान व्यर्थ चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि यह महान् आशा के लिए द्वार बंद कर देता है, मुक्तिदायी कर्म को वर्जित कर देता है, प्रबोधनकारी ज्ञान को बाहर कर देता है। यह एक मिथ्याज्ञान है जो दृश्य जगत् को देखता है पर उस दृश्य जगत् के सत्य को चूक जाता है, एक ऐसी अंधी आशा है जो क्षणभंगुर का पीछा करती है पर सनातन को नहीं देख पाती, एक ऐसा निष्फल कर्म है जिसके प्रत्येक लाभ को उससे होनेवाली हानि लुस कर देती है और जिसका कुल योग केवल सिसिफस (sisyphus) के उस अनंतकालीन परिश्रम के जैसा होता है जिससे हाथ कुछ नहीं लगता है।
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ।। १३ ।।
१३. हे पार्थ! महात्मा, जो दैवी प्रकृति में निवास करते हैं, मुझे उस अविनाशी के रूप में जानते हैं जिससे समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार जानकर वे अनन्य और पूर्ण प्रेम-भक्ति से मेरी ओर मुड़ते हैं।
जो महात्मा अपने-आप को उस दिव्यतर प्रकृति के प्रकाश और विशालता की ओर खोलते हैं, जिसका सामर्थ्य मनुष्य में होता है, वे ही एकमात्र उस पथ पर होते हैं जो आरंभ में बहुत ही सँकरा पर अंत में अत्यंत विशाल होता हुआ मुक्ति और पूर्णता की ओर ले जाता है। मनुष्य के अन्दर निहित देव की वृद्धि करना ही मनुष्य का यथार्थ कर्त्तव्य है; इस निम्नतर आसुरी और राक्षसी प्रकृति का दृढ़ तथा निरंतर भागवत् प्रकृति में परिवर्तन ही मानव जीवन का सतर्कतापूर्वक छिपाया हुआ प्रयोजन है। जैसे-जैसे यह वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे आवरण हटता जाता है और जीव कर्म के महत्तर अभिप्राय को तथा जीवन के यथार्थ सत्य को देखने-समझने लगता है। मनुष्य में निहित भगवान् की ओर, जगत् में निहित भगवान् की ओर दृष्टि खुल जाती है; वह आंतरिक रूप से देखती व बाह्य रूप से जानने लगती है उस अनन्त आत्मा को, उस अविनाशी को जिससे सारे भूत उत्पन्न होते हैं और जो सब भूतों के अन्दर रहता है और जिसके द्वारा और जिसके अन्दर यह सब कुछ सदा अस्तित्वमान रहता है। अतः जब यह दर्शन और यह ज्ञान अंतरात्मा को अधिग्रहीत कर लेता है तब उसकी सारी जीवन-अभिलाषा भगवान् और अनन्त के प्रति अतिशय प्रेम और अथाह भक्ति बन जाती है। तब मन अपने-आप को अनन्य रूप से शाश्वत, अध्यात्मसत्ता, चिरजीवी, विश्वव्यापी, सत् तत्त्व से संबद्ध कर देता है; उसके लिये किसी भी चीज का मूल्य उसी के नाते होता है अन्यथा नहीं, और वह उस सर्वानन्दमय पुरुष में ही आनन्द लेता है।
इसमें मुख्य बात यह है कि भगवान् ही सब कुछ हैं और वे ही सत्य हैं इसलिए उनकी अनन्य रूप से भक्ति करनी चाहिये। और जो उनकी भक्ति नहीं करता वह आसुरिक प्रकृति का है।
प्रश्न : यहाँ उल्लेख है कि पथ आरंभ में बहुत सँकरा होता है, इसका वास्तव में अर्थ क्या है?
उत्तर : हमारे पुराने साहित्यों में भी इसका उल्लेख आता है और श्रीअरविन्द भी उसी बात को यहाँ दोहरा रहे हैं कि पथ आरंभ में बहुत सँकरा और बाद में बहुत विशाल होता जाता है। एक बड़े ही सरल रूपक की सहायता से इसे हम यों समझ सकते हैं कि जब हम अपने निवासस्थान से किसी राजमार्ग के लिए जाते हैं तो प्रायः पहले हमारे घर के सामने मार्ग कुछ सँकरा होगा जो हमें किसी अधिक विशाल मार्ग तक ले जाता है और उससे आगे फिर हम एक अधिक विशाल मार्ग पर या फिर राजमार्ग पर जाते हैं। इसी प्रकार साधना मार्ग भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी सीमा तक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का होता है। प्रत्येक की एक विशिष्ट प्रकार की अभीप्सा होती है। किसी को भगवान् शिव के प्रति अनुराग होता है तो किसी को विष्णु के प्रति। विष्णु के प्रति जिन्हें अनुराग है उनमें भी किसी को उनके किसी रूप विशेष से विशेष लगाव होता है तो किसी दूसरे को उनके किसी दूसरे रूप से। उस रूप विशेष में भी लगाव रखने वालों में यदि हम देखें तो प्रत्येक अपने भिन्न गठन के अनुसार भिन्न-भिन्न तरीके से उसे पूजता है, भिन्न तरीके से उसके पास जाता है। इसलिए जब हम साधना आरंभ करते हैं तो क्या करें और क्या न करें ये नियम बड़े ही सुनिर्धारित, सख्त और बाध्यकारी प्रकार के होते हैं क्योंकि जब हम आरंभ करते हैं तब चेतना इतनी पर्याप्त नमनीय और विशाल नहीं होती कि उसे अधिक छूट दी जा सके। परंतु ज्यों-ज्यों व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए मार्ग पर अग्रसर और विकसित होता जाता है त्यों-ही-त्यों उसके लिए वे नियम फिर उतने कठोर और बाध्यकारी नहीं रह जाते बल्कि अधिक नमनीय होते जाते हैं।
यदि हम अपने मूल स्रोत सच्चिदानंद को देखें तो वहाँ चेतना का अनंत विस्तार है परंतु ज्यों-ज्यों चेतना नीचे उतरती है त्यों-त्यों वह संकीर्ण होती जाती है। जड़-भौतिक तक आते-आते तो वह इतनी संकीर्ण हो जाती है कि लगभग चेतना का विलोम ही प्रतीत होने लगता है। इसलिए जब हम चेतना के इस निचले छोर से अपने मूल स्रोत तक पुनः लौटने की यात्रा आरंभ करते हैं तो स्वाभाविक ही है कि रास्ता आरंभ में सँकरा ही होगा। यह एक देखने का तरीका है। इसे वैदिक रूपक के अनुसार भी देखा जा सकता है। आरंभ में हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में होती हैं, कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर दैवीय शक्तियों की क्रिया बड़ी ही क्षीण रहती है, परंतु ज्यों-ज्यों वह क्रिया बढ़ती जाती है त्यों-ही-त्यों हमारी चेतना विशाल होती जाती है और हमारा कार्यक्षेत्र और प्रभावक्षेत्र अधिकाधिक विशाल होते जाते हैं। इस बात को हम योगी श्रीकृष्णप्रेम के जीवन के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अपनी साधना के आरंभिक समय में उन्होंने वैष्णव उपासना पद्धति और तंत्र के सारे नियमों को अक्षरशः अपनाया और बिल्कुल सख्त रूप से उनका पालन किया। उन्होंने कठोर रूप से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक शुद्धता का पालन किया। जब एक बार उपहासवश छेड़खानी करते हुए किसी ने उनसे कहा कि, "यदि मेरी विधवा दादी इन सब क्रिया-विधि का पालन करती तब तो मैं समझ सकता था, परंतु आपका तो इतना भिन्न अतीत रहा है। पीछे आपके कैम्ब्रीज के दिनों में आपने खूब गोमांस तक भी अवश्य ही खाया होगा! तो आप ये सब शास्त्रसम्मत संयमों का पालन कैसे कर पाते हैं?" इसका उन्होंने जो उत्तर दिया वह बड़ा ही मार्मिक था। उन्होंने कहा, "...मुझे लगता है कि कोई भी आत्म-आरोपित अनुशासन, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, आज के समय में एक बहुत अच्छी चीज है जब कि हर प्रकार का सामाजिक या व्यक्तिगत अंकुश या संयम खिड़की से बाहर फेंक दिये जाने की प्रक्रिया में है। और साथ ही इसलिए क्योंकि बस यही वह पथ है जो उनके द्वारा तैयार किया गया है जो मेरे से पहले जा चुके हैं और लक्ष्य तक पहुँच चुके हैं। अभी-अभी पथ पर प्रवेश किया हुआ मैं यह कहने वाला होता कौन हूँ कि 'मैं यह करूँगा और वह नहीं, यह अनुशासन तो स्वीकार करूंगा परंतु वह नहीं?' मैं तो पूरे का पूरा ही स्वीकार करता हूँ।"* और वास्तव में उनका पूरा जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण था। उन्हीं के जीवन वृत्तांत में हम पाते हैं कि किस प्रकार बाद के समय में उन्होंने अपने बाह्य अनुशासनात्मक नियमों को बहुत कुछ नमनीय और सर्वसमावेशी बना दिया। इसी से हमें इस बात का पता लगता है कि किस प्रकार पथ आरंभ में संकीर्ण होता है पर बाद में अत्यधिक विशाल बन जाता है।
योग की विभिन्न विचारधाराओं में हम पाते हैं कि उनमें से अधिकांश कुछ संकीर्ण या एकांगी विषय पर आकर रुक जाती हैं परंतु गीता के निरूपण में हम पाते हैं कि वह सभी विचारधाराओं और पद्धतियों को प्रतिध्वनित करती हुई उन सभी का समन्वय साध देती है और अन्त में उन सबकी सीमाओं को तोड़ कर 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' का उपदेश करती है। गीता के ऐसे विकासक्रम के विषय में जब किसी ने श्रीअरविन्द से पूछा कि गीता ने अपना परम रहस्य 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' आरंभ में ही क्यों नहीं दे दिया, तब इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि धर्मों को त्यागने के लिए पहले व्यक्ति के पास कोई धर्म तो होने चाहिये। इसीलिए व्यक्ति को पहले विभिन्न धर्मों की सहायता से, अर्थात् विभिन्न मानसिक, मनोवैज्ञानिक आधारों पर अपने आपको विकसित करना होता है और जब एक बार उसका भली-भाँति विकास हो जाए तभी तो वह उनका त्याग करने की स्थिति में होगा। अन्यथा बिना पहले उन धर्मों को अपनाए वह उनका त्याग कर ही कैसे सकता है। इसी प्रकार, श्रीअरविन्द कहते हैं कि मनुष्य के विकास में अहं पहले सहायक होता है और फिर जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तब उससे ऊपर उठा जा सकता है।
चेतना के विकासक्रम में भी हम देख सकते हैं कि जड़भौतिक पदार्थ पूर्ण रूप से नियमों से बँधा हुआ है और ज्यों-ज्यों हम चेतना के उच्चतर स्तरों पर आरोहण करते हैं त्यों-त्यों अधिक स्वतंत्रता आती जाती है। जड़भौतिक से अधिक स्वतंत्रता प्राण में होती है और उससे अधिक मन में होती है। इस प्रकार इन सभी तरीकों से हम देख सकते हैं कि आरंभ में चेतना संकीर्ण होती है और उत्तरोत्तर विकास के साथ वह अधिकाधिक विशाल होती जाती है।
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
नमस्यन्तश्व मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ।। १४।।
१४. मेरी दिव्य कीर्ति का सतत् स्तवन करते हुए, आध्यात्मिक यत्न में दृढ़ स्थित होकर, मेरे आगे नतमस्तक होकर, नित्य योग युक्त होकर वे भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं।
समस्त वाणी और संपूर्ण चिंतन उस विश्वव्यापी महत्ता, प्रकाश, सौन्दर्य, शक्ति और सत्य का एक स्तुति-गान बन जाता है जिसने अपनी महिमा सहित अपने-आप को उस मानव-आत्मा के समक्ष प्रकट किया है और यही उसकी उन एकमेव परम् आत्मा और अनन्त पुरुष की उपासना होती है। बाह्य प्रस्फुटन के लिए अंतःसत्ता का सुदीर्घ काल से चला आ रहा दबाव अब अंतरात्मा में भगवान् को प्राप्त करने और प्रकृति में भगवान् को सिद्ध करने की एक आध्यात्मिक चेष्टा और अभीप्सा का रूप धारण कर लेता है। संपूर्ण जीवन उन भगवान् और इस मानव-आत्मा का सतत् योग और एकीकरण बन जाता है। यही सर्वांगीण भक्ति का कार्य-स्वरूप है; समर्पित हृदय से शाश्वत पुरुषोत्तम के प्रति यज्ञ के द्वारा यह हमारी समस्त सत्ता और प्रकृति का एक साथ उत्थान साधित कर देता है।
----------------------------------------
* योगी श्रीकृष्णप्रेम, पृष्ठ xviii
इसी कारण हमारे पुराणों में जिस रूप में वैदिक सत्य का निरूपण हुआ है वह मानव सत्ता के विभिन्न भागों के लिए उस सत्य को ग्राह्य बना देता है। वेदों में जिस रूप में उसका निरूपण हुआ है वह तो बिना अंतर्बोध के सुगम नहीं है। परंतु पुराणों में कथाओं, रूपकों आदि अनेक माध्यमों से उसी सत्य का निरूपण हुआ है जिसका कि पठन, श्रवण, चिंतन, गायन आदि करने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह हमारे विभिन्न भागों पर अपना प्रभाव डालता है। इसीलिए कथा-श्रवण, सप्ताह यज्ञ आदि का इतना भारी महत्त्व रहा है। क्योंकि भले ही कोई बौद्धिक रूप से समझे या न समझे, पर व्यक्ति उससे भावनात्मक रूप से अवश्य ही कुछ न कुछ ग्रहण करता है। इसी कारण यह प्रसंग आता है कि वेद, उपनिषद् व अन्य पुराणों की रचना करने के बाद भी जब वेदव्यासजी असंतुष्ट थे तब नारद जी ने उन्हें श्रीमद्भागवत की रचना करने को कहा क्योंकि उसी के द्वारा हृदय, भावनात्मक भाग तथा हमारे अन्य भाग अपने-अपने तरीके से भगवान् के संपर्क में आकर परिपुष्ट हो सकते हैं अन्यथा केवल कोरे ज्ञान की बातों में उन्हें कोई रस नहीं आता और न ही उससे उनकी पुष्टि होती है। जब तक भगवान् की लीला-कथाओं का वर्णन न हो, उनका गान न हो तब तक हमारी क्रियात्मक, भावात्मक, सौंदर्यग्राही, सुखभोगवादी प्रकृति को प्रभावित नहीं किया जा सकता। केवल कोरे ज्ञान से हमारी प्रकृति के इन भागों को सक्रिय नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें किसी चीज के विषय में ज्ञान होने पर भी व्यवहार में हम उस दिशा में अधिक कुछ कर नहीं पाते। वहीं एक बार जब हमारे हृदय को छू दिया जाता है तब हम पूरे मनोयोग से किसी उद्देश्य के लिए परिश्रम करने को, अपनी ऊर्जा लगाने को सहर्ष तैयार हो जाते हैं। और जब एक बार हमारे कुछ भाग उन लीला कथाओं में आनंद अनुभव करने लगते हैं तब निम्न वृत्तियों की निरंकुश क्रीड़ा पर इससे बहुत कुछ अंकुश और अनुशासन आने लगता है। केवल मानसिक समझ से यह संभव नहीं है। यहाँ तक कि अनेक वर्षों तक साधना करते रहने पर भी हमारे अंदर ऐसे हिस्से छिपे रह सकते हैं जिन्हें साधना से, भगवान् से, अपने इष्ट से कोई मतलब नहीं होता। वे तो अपने ही सुख के साधनों को खोजने में लगे रहते हैं। किसी को परिवार में सुख मिलता है, किसी को अपनी पद-प्रतिष्ठा में सुख मिलता है, किसी को जीभ के स्वाद की तथा अन्य शारीरिक विलासिता के साधनों की पूर्ति में सुख मिलता है। ऐसा कौन साधक होगा जिसमें कि ये हिस्से बहुत दीर्घ काल तक भी अंदर छिपे न रहते होंगे और साधना में कदम-कदम पर उसे अपने उद्देश्य से विभ्रमित और विचलित करने का प्रयास न करते होंगे। इन सभी हिस्सों को प्रत्येक साधक अपने-अपने तरीके से संयमित करने का प्रयास करता है। परंतु यह प्रकृति ऐसी दुःसाध्य है कि साधनापथ में यह आम बात है कि व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए यदि मन परमात्मा के कीर्तन में, उनके स्तवन में लग जाए तो यह एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। सामान्यतः तो हमें यह देखने को ही नहीं मिलता कि व्यक्ति को भगवान् की लीला कथाओं में, उनके स्तवन आदि में ही रस आता हो। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं और वास्तव में ही उन्हें लगता भी है कि उनका मन भगवान् में लग रहा है और वे उनका भजन-कीर्तन करना चाहते हैं, परंतु एक निश्चित समय सीमा के बाद वे उस सब से ऊब जाते हैं और तब उन्हें अन्य वे सब साधन चाहिये जिनमें उनका मन वास्तव में लगता है। अधिकांश को लगता है कि भगवान् का भजन करना भले ही एक अच्छी चीज है परंतु वह भी मर्यादित समय सीमा में ही अच्छा है क्योंकि व्यावहारिक जीवन में अन्य दायित्व भी हैं जिनका उन्हें निर्वाह करना पड़ता है। इस प्रकार की मानसिकता में तो व्यक्ति को यह आभास ही नहीं होता कि उसका मन वास्तव में भगवान् के स्तवन में लगता ही नहीं है। जब इस दृष्टिकोण से हम गीता की बात को समझें तब हमें अनुभव होगा कि गीता कितनी गंभीर बात कर रही है। गीता जिस चिंतन की बात करती है वह सतत् चिंतन की बात है। वह कोई समय विशेष का ध्यान, पूजा, अनुष्ठान आदि नहीं है। अतः यदि किसी के अंदर यह सतत् चिंतन सक्रिय हो जाए तो यह एक बहुत बड़ा रूपांतर साधित हो जाता है। यदि इस दृष्टिकोण से इसे न देखें तो हम भ्रमित हो सकते हैं कि अक्षर ब्रह्म के ज्ञान की बात करने के बाद अब गीता ऐसे कनिष्ठतर विषयों की बात क्यों कर रही है। परंतु जब सही परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को समझेंगे तब हम पाएँगे कि यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस सतत् चिंतन के आने पर ही वास्तव में ज्ञानयज्ञ हो सकता है।
अधिकांशतः तो व्यक्ति जिसे ज्ञान कहता है उसे इसीलिए चाहता है कि उसके द्वारा उसकी साधना हो जाए, उससे सुख प्राप्त हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, आदि-आदि। परंतु यह ज्ञानयज्ञ नहीं है। ऐसे मनोभाव में तो यज्ञ का आरंभ ही नहीं हुआ होता। ज्ञानयज्ञ तो तब आरंभ होता है जब व्यक्ति जानना केवल इसलिए चाहता है कि उससे वह भगवान् की सेवा अधिक अच्छे ढंग से कर सके। उससे अधिक जानने से उसे कोई सरोकार नहीं होता। अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए उसे ज्ञान की कोई चाह नहीं होती। यदि कहने को व्यक्ति वेद-वेदांत आदि में पारंगत भी हो जाए परंतु उसकी सहायता से वह एक कदम भी परमात्मा की ओर गति न कर सकता हो तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। ज्ञानयज्ञ का अर्थ है कि व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञान भगवान् की, श्रीमाताजी की सेवा में अर्पित हो जाता है। सच्चा ज्ञान इस भाव में निहित है कि भगवान् जो कराएँ, जैसा ज्ञान दें, जैसे भी रखें वही सही है बाकी सब निरर्थक है। अन्यथा तो ज्ञान के नाम पर केवल अहं का ही पोषण होता है। यही नहीं, जितना ही वह बढ़ता है उतनी ही अहंकेंद्रितता भी बढ़ती जाती है क्योंकि व्यक्ति उस ज्ञानाभिमान के दंभ से अधिकाधिक फूलने लगता है। यज्ञ का अर्थ है पवित्र बनाना। साधना, ज्ञान, भक्ति, कर्म आदि सभी बातें तब तक बिल्कुल बेकार और अपवित्र हैं जब तक कि वे प्रभु के चरणों में समर्पित न हो जाएँ। अधिक से अधिक केवल यह संभव है कि ये सब चीजें मनुष्य को सत्त्व की ओर ले जाएँ, परंतु इससे कोई सच्ची उपलब्धि नहीं हो जाती क्योंकि सत्त्व भी तो एक जंजीर ही है। आत्मज्ञान आदि का प्रयास तो व्यक्ति को सात्त्विक ही बना सकता है, परंतु, जैसा कि श्रीकृष्णप्रेम कहते थे, मुकुंद की सेवा ही है जो निखैगुण्य है। और ऐसे सच्चे सेवा के मनोभाव में ही सच्चा ज्ञान आ सकता है। यदि यह मनोभाव न हो तो व्यक्ति में केवल भेदबुद्धि ही बनी रहती है और वह अहं पर ही केंद्रित रहता है। परंतु इस मनोभाव के आने में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं हमारे मन, प्राण और शरीर की वृत्तियाँ। किसी को परिवार में सुख मिलता है और वह उसे छोड़ नहीं सकता, किसी को संपत्ति से लगाव है, किसी को अपनी यश-कीर्ति, बड़ाई, पद-प्रतिष्ठा में रुचि है, वहीं किसी को अपनी भोग-विलासिता में ही आनंद आता है। कोई विरला ही है जो वास्तव में इनके पाश से छूट कर किसी सच्ची चीज की ओर चल पाए। इन सबकी माया ऐसी सम्मोहित कर देती है कि इनकी पाश में बंधे होकर भी व्यक्ति को ऐसा भ्रम हो सकता है कि उसका मन तो भगवान् में लगता है, कि वह साधना कर रहा है, या ऐसे ही अन्य कोई विचार। इसलिए गीता अब जिस चीज का निरूपण कर रही है वह एकांगी कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि से भी बड़ी श्रेष्ठतर स्थिति है जिसमें व्यक्ति का मन भगवान् के सतत् स्तवन में लग जाता है।
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ।। १५।।
१५. और अन्य दूसरे जन मुझे मेरे एकत्व भाव में, प्रत्येक पृथक् जीव में (पृथक् भाव में) और मेरे समस्त असंख्य वैश्व चेहरों में ज्ञानयज्ञ के द्वारा खोजते हैं (मेरा यजन करते हैं) और मेरी उपासना करते हैं।
जो लोग ज्ञान पर ही अधिक बल देते हैं, वे भी अंतरात्मा और प्रकृति पर होनेवाले भगवान् के दर्शन की निरंतर बढ़नेवाली, अपने अन्दर लीन करनेवाली और अपने रास्ते पर चलानेवाली शक्ति के द्वारा उसी बिंदु पर पहुँचते हैं। उनका यज्ञ ज्ञान-यज्ञ होता है और ज्ञान के ही एक अनिर्वचनीय आनंद के द्वारा वे पुरुषोत्तम की भक्ति पर पहुँच जाते हैं, ज्ञानयज्ञेन यजन्तो मामुपासते। यह वह ज्ञान है जो भक्ति से परिपूर्ण है, क्योंकि यह अपने साधनों में पूर्ण है, अपने लक्ष्य में पूर्ण है। यह परमोच्च को मात्र एक अमूर्त एकत्व अथवा अनिर्धार्य या बुद्धि से अग्राह्य निरपेक्ष सत्ता के रूप में मान कर उसकी खोज करना नहीं है। यह तो परमोच्च की और वैश्वसत्ता की हार्दिक खोज और उन्हें अधिकृत करना है; यह अनन्त को उनकी अनन्तता में, और अनन्त को जो कुछ सीमित है उस सब में ढूँढ़ना है; यह उन 'एक' को उनके एकत्व में और उन्हीं 'एक' को उनके अनेकविध तत्त्वों में, उनकी असंख्य छवियों, शक्तियों और रूपों में, यत्र-तत्र-सर्वत्र, कालातीतता में और काल में, गुणन में, विभाजन में, उनके ईश्वरभाव के अनन्त पहलुओं में, असंख्य जीवों में, उनके उन करोल विश्वरूपों में जो जगत् और उसके प्राणियों के रूप में हमारे सामने हैं, एकक्क पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्, देखना और आलिंगन करना है। यह जार सहज ही एक आराधन, एक व्यापक भक्ति, एक विशाल आत्मदान, एक सर्वांगीण आत्मोत्सर्ग बन जाता है क्योंकि यह उस आत्मा का ज्ञान है, उस आत्मसत्ता का संस्पर्श है, उस परम और विराट् पुरुष का आलिंगन है जो हमें हम जो कुछ भी हैं उसे, अपना बना लेता है और साथ ही जब हम उसके समी पहुँचते हैं तो हमारे ऊपर सत्स्वरूप के अनन्त आनन्द की निधियाँ बरसाता है।
ज्यों-ज्यों व्यक्ति को भक्तिपूरित ज्ञान होता है वह सर्वत्र ही ईश्वर के दर्शन करने लगता है और उनसे प्रेम करने लगता है। और जब व्यक्ति सर्वत्र उनसे प्रेम करता है तब वे भी उसके समक्ष अपने विभिन्न रूप, अपने विभिन्न पहलू प्रकट करना आरंभ करते हैं। परंतु यह ज्ञान, यह प्राकट्य केवल भक्ति के प्रभाव से ही आता है। इस प्रकार भक्ति के प्रभाव से हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, हमारे सभी भाव एकांगी न रहकर समग्र और व्यापक स्वरूप धारण कर लेते हैं और इस समग्रता में उत्तरोत्तर पराभक्ति की ओर वृद्धि करते हैं। पराभक्ति का अर्थ है 'सर्वभावेन' अर्थात् व्यक्ति अपने सभी भावों को अनन्य रूप से भगवान् की भक्ति में परिणत कर देता है। तब कर्म, ज्ञान आदि सभी केवल प्रभु के प्रीत्यर्थ निवेदित होते हैं और वे सभी अहं की तुष्टि की बजाय भगवान् की भक्ति के साधन बन जाते हैं। तब व्यक्ति को स्वयं के लिए या उनके अपने लिए ज्ञान से या कर्म से कोई रुचि नहीं रहती अपितु ये तो उस भक्ति से ही उद्भूत होते हैं। कर्म भी उस भक्ति के अनुरूप ही उद्भूत होते हैं और ज्ञान भी उसी के अनुरूप प्रस्फुटित होता है। तब ये सभी भाग भिन्न स्वर न रहकर समस्वर बन जाते हैं।
सच्चे ज्ञान और सच्चे कर्म का उद्भव भगवान् के प्रति समर्पित हृदय के द्वारा ही हो सकता है अन्यथा अन्य किसी तरीके से वे पूरी तरह प्रस्फुटित हो ही नहीं सकते। जब पराभक्ति आ जाती है तभी दिव्य कर्म और दिव्य ज्ञान संभव हैं अन्यथा नहीं। यही चेतना की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति यदि घोर से घोर कर्म भी करे तो भी वे उसे बाँधते नहीं और न ही वह ज्ञान बंधनकारी होता है क्योंकि व्यक्ति को अपने आप में न तो उस कर्म से कुछ हेतु सिद्ध करना होता है और न ही उस ज्ञान से। यदि भक्ति न हो तो कर्म और ज्ञान के बाहरी स्वरूप भले जो भी क्यों न हों, चाहे कितने भी सूक्ष्म रूप से ही क्यों न हों परंतु वे रहते हैं केवल अहं की तुष्टि के साधन ही। इसीलिए भक्ति आने पर सच्चा ज्ञान तो स्वयमेव ही आ जाता है क्योंकि भक्ति तो ज्ञान की परिणति है और संपूर्ण कर्मों का आधार है। अन्यथा जिसे हम भक्ति कहते हैं वह तो भगवान् की नहीं अपितु अपने अहं की ही भक्ति होती है जिसे हम अनेक सुंदर-सुंदर नामों से सजा देते हैं। परंतु जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह श्रीमाताजी के हाथों में सौंप देता है तब वे ही उसके लिए ज्ञान, कर्म आदि जो भी सच्चे रूप से आवश्यक हैं वे स्वयं ही उत्पन्न कर देती हैं और उसे मार्ग पर आगे ले चलती हैं। जब एक बार व्यक्ति को यह सच्ची समझ आ गई कि एकमात्र श्रीमाताजी ही जीवन में अनुगमन करने योग्य हैं और बाकी सब तो निरर्थक है, तो यही परम ज्ञान है। इसके बाद तो केवल व्यावहारिक तौर पर इस ज्ञान को मन, प्राण आदि के माध्यम से अभिव्यक्त करने का विषय रह जाता है, वास्तव में जो मूलभूत काम है वह तो हो ही जाता है। हालाँकि शुद्ध रूप से इसे अभिव्यक्त करने में भी अपनी भीषण चुनौतियाँ हैं, परंतु वे सभी चुनौतियाँ एक सही दिशा में होती हैं अन्यथा तो व्यक्ति को दिशा ही प्राप्त नहीं होती और जीवन निरुद्देश्य ही बीत जाता है। इसलिए इस सब का हमारे लिए व्यावहारिक संदेश यही है कि हम अपनी सारी शक्ति-सामर्थ्य, हमारे सारे गुण-अवगुण, अपना सर्वस्व अपने अहं की बजाय श्रीमाताजी की सेवा में समर्पित कर दें, अन्यथा तो साधना भी अपने आप में एक बोझ ही है जो कि जितना एक सामान्य मनुष्य स्वयं पर केंद्रित नहीं होता उससे अधिक एक साधक को स्व-केंद्रित बना देती है। सामान्यतः साधनामय जीवन व्यतीत करने के नाम पर प्राण अपने व्यापार का और अधिक प्रसार कर देता है क्योंकि तब व्यक्ति पहले की अपेक्षा और अधिक आत्माभिमान से फूल उठता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। गुरु के पास भी यदि वह जाता है तो इस भाव से कि उसे गुरु से क्या आत्मिक, मनोवैज्ञानिक, प्राणिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त तो कोई अहंकेंद्रित व्यक्ति कुछ सोच ही नहीं सकता। इसमें कोई दोष की बात भी नहीं है क्योंकि हमारा प्राकृत गठन ही इस प्रकार का होता है कि प्रारंभ में बिना लेन-देन, लाभ-हानि या स्वकेंद्रितता के भाव के हम और कुछ कर या सोच ही नहीं सकते। इसीलिए जो साधना पथ पर आ जाते हैं ऐसे हजारों व्यक्तियों में से भी कोई विरला ही वास्तव में किसी सच्ची स्थिति तक पहुँचता है।
अब ज्ञान को आधार प्रदान करने के लिए श्रीभगवान् घोषित करते हैं कि वे ही सब कुछ हैं। एक सच्चे दृष्टिकोण से देखें तो जब तक व्यक्ति को दूसरे के अंदर भगवान् के या फिर अपने इष्ट के दर्शन नहीं होते तर तक तो वह केवल भ्रम में ही है क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त तो अन्य किय की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इसलिए किसी दूसरे का भला करने का भी एकमात्र जो सच्चा तरीका है और वह है अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान् को, अपने गुरु को समर्पित कर देना। यदि व्यक्ति सब में परमात्मा का दर्शन न कर के अपने से भिन्न सत्ता देखता है तो यह तो स्वयं की सत्ता के मूलभूत सत्य का ही निषेध है, खंडन है। हालाँकि सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होने का अर्थ यह नहीं है कि तब कोई पृथक्ता का बोध हो नहीं रहता और सभी कुछ आपस में इस प्रकार घुल-मिल जाता है मानो कोई वैविध्य ही न रहा हो। सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होने की बात का हमारी बुद्धि सामान्यतः ऐसा ही अर्थ लगाती है। वास्तव में तो जब व्यक्ति को सर्वत्र वह दर्शन प्राप्त होता है तभी वह सच्चे रूप से हर चीज के साथ व्यवहार और क्रिया कर सकता है। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति सर्वभूतों के सच्चे हित में रत रह सकता है। चूंकि भगवान् ही सभी कुछ के आधार हैं इसलिए जब व्यक्ति अपने आप को उन्हें समर्पित कर देता है और उन्हीं की सेवा में रत रहता है तो स्वतः ही वह तो सभी कुछ के कल्याण में रत है।
प्रश्न : इसका अर्थ है कि गृहस्थ व्यक्ति तो कभी भक्ति कर ही नहीं सकता?
उत्तर : क्या नरसी मेहता, मीराबाई, गुरु नानक देव आदि के परिवार नहीं थे? श्री रामकृष्ण परमहंस के परिवार नहीं था? परंतु जो परिवार में हो लिप्त रहता है उसकी तो भक्ति परिवार के प्रति ही हुई। अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना परिवार का हो। हम अनेकानेक ऐसे उदाहरण पाते हैं जो कि परिवार में रहते हुए भी भगवान् के भक्त हुए हैं। यह चीज इस पर निर्भर नहीं करती कि व्यक्ति का परिवार है या नहीं, या फिर वह किस प्रकार की बाहरी क्रियाकलाप करता है, परंतु सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि चेतना का स्तर और उसकी स्थिति क्या है, परिवार के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। इसलिए जो भगवान् के भक्त होते हैं उनकी चेतना परिवार में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ी होती है। क्या हम गुरु नानक की चेतना परिवार से बंधी हुई कह सकते हैं या फिर मीराबाई की चेतना की तुलना किसी सामान्य घरेलू स्त्री की चेतना से कर सकते हैं।
प्रश्न : परंतु चेतना की वह स्थिति भी तो तभी होगी जब परमात्मा की कृपा होगी। अपने आप तो वह चेतना आ नहीं जाती।
उत्तर : इस कृपा शब्द की आड़ में हम अपनी अकर्मण्यता को ही उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। अब व्यक्ति कहेगा कि उसके ऊपर तो भगवान् की कृपा नहीं है इसलिए वह भक्ति किस प्रकार करे। यह तो भगवान् के प्रति दुर्भावना की बात हुई। यदि व्यक्ति में इतनी सच्चाई हो कि बुद्धि से उसे जो कुछ समझ में आ जाता है उसे वह अपनी यथाशक्ति चरितार्थ करने का प्रयास करता है पर अभी तक भक्ति का उदय न होने के कारण वह नहीं जानता कि उसका अनुसरण किस प्रकार करे, तो यह एक अलग विषय हो सकता है। परंतु कोई एक व्यक्ति भी यह नहीं कह सकता कि उसे बुद्धि से जो चीज समझ आ गई है उसे चरितार्थ करने के लिए वह प्रयत्न नहीं कर सकता। यदि एक बार उसके समझ में आ जाए कि अमुक काम करने योग्य है तो उसे उसकी चरितार्थता के लिए आवश्यक संकल्प और साधन आदि जुटाने चाहिये। सच्चाई इसमें है कि जब एक बार व्यक्ति को कुछ समझ में आ जाए तब उसे करने का वह यथाशक्ति प्रयास करे। यदि शिक्षक विद्यार्थी को हल करने के लिए गणित का कोई सवाल दें परंतु वह यह कह कर प्रयास करने से ही इंकार कर दे कि गुरुजी की कृपा होगी तो प्रश्न स्वयं ही हल हो जाएगा तो यह एक बिल्कुल बेतुकी बात होगी। इसलिए सामान्यतः ये जो आम प्रचलन की बातें हैं वे केवल ऐसे बहाने मात्र हैं जिनकी आड़ में हम अपनी दुर्भावना और अपने आलस्य को और अपनी अकर्मण्यता की वृत्ति को छिपाते हैं। यदि हमारा कोई प्रिय या सगा-संबंधी गंभीर रूप से बीमार होता है तब हम उसे बचाने के यथासंभव प्रयास करते हैं, और तब हम कृपा शब्द का दुरुपयोग करते हुए यह नहीं कहते कि भगवान् की कृपा होगी तो वह स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार जहाँ कहीं हमारे निजी लाभ या हानि निहित होते हैं उन सब चीजों में हम अपना पूरा मनोयोग लगा देते हैं। ऐसे मामलों में हम कभी किसी को कृपा के सहारे चीजों को छोड़ते नहीं देखते। परंतु जहाँ कहीं व्यक्ति आवश्यक श्रम से बचना चाहता है वहीं अधिकांशतः वह इस शब्द का दुरुपयोग करता है। भगवान् तो हर स्थिति में कृपा ही करते हैं। हमारे लिए जो लाभदायक होता है उसमें भी उनकी उतनी ही कृपा होती है जितनी की उसमें जो हमें हानिकारक प्रतीत होता है। इसलिए कृपा तो एक ऐसी मूलभूत चीज है जो हमारी किन्हीं भी बाहरी अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती। वह तो हर हालत में, हर चीज के पीछे, हर घटना के पीछे स्वतः विद्यमान है। इसलिए हमारे सभी ग्रंथों में हम देखते हैं कि भगवान् के तो अनुग्रह में भी उतनी ही कृपा होती है जितनी कि संहार में। भगवान् जिसका संहार करते हैं उसकी जैसी सद्गति होती है वैसी तो योगियों-तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए भगवान् की कृपा तो निर्विवाद रूप से हर हालात में है ही क्योंकि वे स्वयं ही तो विद्यमान हैं इसलिए वे अपने आप के ऊपर कृपा के अतिरिक्त और कुछ कर भी क्या सकते हैं। वास्तव में तो हमारे चारों ओर कृपा के समुद्र भरे हुए हैं परंतु हमने अपने आप को सतर्कतापूर्वक इतना बंद कर रखा है कि कहीं से कृपा की कोई बूँद प्रवेश न करने पाए। इसलिए करने का काम केवल एक ही है कि हमने अहं पर केंद्रित होकर जो द्वार बंद कर रखे हैं उन्हें खोलें ताकि कृपा और प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर सकें।
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ।। १६ ।।
१६. मैं यज्ञकर्म हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही अन्न की भेंट (स्वधा) हूँ, मैं हो अग्निदायी औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं हो आहुति हूँ।
कर्म का मार्ग भी आत्मनिवेदनरूपी उपासना और भक्ति में परिणत हो जाता है क्योंकि यह हमारे संकल्प और उसकी सारी क्रियाओं का उन एकमेव पुरुषोत्तम के प्रति पूर्ण यज्ञ अर्थात् समर्पण होता है। बाह्य वैदिक यज्ञ-अनुष्ठान एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो हो भले ही अल्प उद्देश्य के लिए पर फिर भी स्वर्गमुखी उद्देश्य की ओर कारगर है; परंतु वास्तविक यज्ञ तो वह आंतरिक होम है जिसमें 'समय भगवान्' स्वयं ही यज्ञ-क्रिया, यज्ञ और यज्ञ को प्रत्येक बस्तु और घटना बन जाते हैं। इस आंतर यज्ञविधि की सारी क्रियाएँ और अनुष्ठान हमारे अन्दर उन्हीं की शक्ति का आत्म-विधान और आत्माभिव्यक्ति होते हैं। यह शक्ति हमारी अभीप्सा के द्वारा अपनी ऊर्जा के स्रोत की ओर ऊपर बढ़ती जाती है। दिव्य अंतःवासी स्वयं यज्ञ की अग्नि और हवि बनते हैं. कोल हैं। अनि भगवन्मुखी संकल्प है और स्वयं भगवान् ही हमारे यह संकल्प होते हैं। और, हथि भी हमारी प्रकृति तथा सत्ता के अन्तःस्थ भगवान् का ही रूप और शक्ति है; जो कुछ उनसे प्राप्त हुआ है वह उन्हीं के सत्स्वरूप, उन्हीं के परम सत्य और मूलस्रोत की सेवा और पूजा में भेंट चढ़ाया जाता है। दिव्य मनीषी-कवि स्वयं ही पवित्र मंत्र बन जाते हैं; यह उन्हीं की सत्ता की ज्योति है जो भगवन्मुखी विचार के रूप में अपने-आप को अभिव्यक्त करती है और उस प्रकटनकारी तेजोदीप्त शब्द (मंत्र) में प्रभावी होती है जो कि विचार के गूढ़ रहस्य को मंडित किये रहता है...
यह सारा तो वैदिक प्रतीक है कि किस प्रकार हमारा समस्त कर्म यज्ञ रूप होकर भगवान् को समर्पित हो जाता है। 'अग्नि' भागवत् संकल्प का प्रतीक है। अग्नि में हवि समर्पित करने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं-कामनाओं आदि को उस भागवत् संकल्प के अंदर समर्पित करता है। कुछ सामग्री ऐसी होती है जो अग्नि में डालने पर धुँआ पैदा करती है। हमारे आवेग और अंध संवेग ही यह धुँआ है। इसलिए ऐसी सामग्री को भली-भाँति जलाने के लिए घृत की आवश्यकता होती है। घृत है विशुद्धिकृत बुद्धि। घृत हमें मिलता है 'गो' अर्थात् प्रकाश से। जब विशुद्ध बुद्धि होगी तभी हमारी अंध वृत्तियों का भगवतोन्मुख हवन हो सकता है अन्यथा तो ये अंध वृत्तियाँ अपने-अपने निहित हेतुओं को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होतीं और सदा अपने ही तरीके से चीजों को चाहती हैं और केवल अपनी ही तुष्टि चाहती हैं। जब विशुद्ध बुद्धि आती है तब इन अंध वृत्तियों पर अंकुश लगने लगता है और वह बुद्धि इन सब को उस भागवत् संकल्प में होम कर देती है जो यहाँ अभिव्यक्त होना चाह रहा है। हमारा सच्चा विकास, हमारी सच्ची शुद्धि तभी होगी जब हमारी सत्ता अग्नि में हवन - अर्थात् भागवत् संकल्प के प्रति समर्पित - होगी। इसी से कर्म योग बन सकता है।
भगवान् को समर्पित होने पर ही हमारे कर्म योग का रूप लेते हैं अन्यथा तो वे योग नहीं अपितु रोग होते हैं। अधिकांशतः तो हमारे कर्म केवल हमारे कामपुरुष की तुष्टि और उसी की अभिव्यक्ति होते हैं। हमारे सभी कर्म सामान्यतः किसी कामना की पूर्ति के लिए, अपने अहं की तुष्टि के लिए, या अधिक से अधिक किसी सात्त्विक चेष्टा को पूरा करने के लिए किये जाते हैं। इनमें से कोई भी कर्म हमें ऊपर नहीं लेकर जाते। इन सब की अपनी-अपनी सीमाएँ हैं और ये उन्हीं सीमाओं के भीतर रहते हैं। यज्ञ रूप से, परमात्मा की ओर जाने के साधन के रूप में जब कर्म किया जाता है तब वह सच्चा कर्म होता है। पर कर्म की मुख्य ग्रंथि है कामना, और जब तक उस ग्रंथि को सुलझाया नहीं जाता तब तक सच्चा कर्म संभव नहीं है।
प्रश्न : पर ये कामना के विचार आते कहाँ से हैं जबकि कई चीजें के विषय में तो हम सोचते ही नहीं हैं और फिर भी व्यवहार में हम वैर्मी चीजें कर बैठते हैं?
उत्तर : जब सामान्यतः हम कहते हैं कि 'हम ऐसा नहीं सोचते' तो वह हम अपनी बुद्धि के बारे में कहते हैं, क्योंकि वास्तव में ही हम बुद्धि से वैसी चीजें नहीं सोच रहे होते। परंतु हमारी बुद्धि क्या सोचती है उससे हमारी प्राणिक सत्ता को कोई विशेष सरोकार नहीं है। उसके अपने निहित हेतु होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वह हमारी इंद्रियों को, भावों, संवेदनों आदि पर अधिकार करके उन्हें अपने हेतु सिद्ध करने के काम में लेती है। इसी कारण व्यक्ति सोचता एक चीज है परंतु वास्तव में करता कुछ और है। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान् अर्जुन को कहते हैं कि 'महत्तर आत्मा के द्वारा निम्नकोटि के स्व को स्थिर निश्चल कर के कठिनाई से पकड़ में आने वाले कामनारूप शत्रु को मार डाल।' अहं के बिना कामना नहीं हो सकती। अतः जब अहं, कामना, गुण और द्वंद्व रूपी प्रपंच चल रहा होता है तब ऐसे में यदि बुद्धि किसी चीज का निषेध करती है, किसी चीज के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करती भी है तो भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपनी बुद्धि में तो इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट होते हैं कि भगवान् की ओर जाना ही श्रेष्ठ है परंतु फिर भी व्यावहारिक रूप से उस ओर एक कदम भी नहीं उठा पाते।
प्रश्न : तो जब व्यक्ति में दृढ़-संकल्प हो तब क्या इस तरह के कामना आदि के विचार नहीं उठते?
उत्तर : विचार तो उठते ही हैं क्योंकि जब तक उपद्रवी तत्त्व हमारी सत्ता में होंगे तब तक कोलाहल, उपद्रव आदि तो होंगे ही। परंतु संकल्प की शक्ति से व्यक्ति उन्हें धीरे-धीरे अनदेखा करता है। यदि व्यक्ति उन्हें अपने से विजातीय तत्त्व समझ कर दूर धकेलता है तब तो वे उसके ऊपर अधिक हावी नहीं हो पाते, परंतु यदि वह उन इच्छाओं, कामनाओं आदि को अपनी निजी चीजें समझ कर उनमें रस लेने लगता है तो वे हावी हो जाती हैं। कामना आदि के विषय में तो श्रीमाताजी कहती हैं कि भले हो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वे उसके अपने अंदर उत्पन्न होती हैं परंतु वास्तव में तो बाहर उनका एक समुद्र होता है जिसमें से वे उठती हैं और अपनी तुष्टि के माध्यम ढूँढ़ती हैं। यदि व्यक्ति उनको अभिव्यक्ति प्रदान करने से इंकार करे तो एक बार तो वे अपनी अभिव्यक्ति के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाती हैं परंतु अभिव्यक्ति का अवसर न मिलने पर एक समय के बाद निराश हो जाती हैं और उस व्यक्ति को छोड़ देती हैं।
प्रश्न : परंतु ऐसे कुछ विचार होते हैं जिनके विषय में हम न तो सोचते हैं न कल्पना ही करते हैं, वे कहाँ से आते हैं?
उत्तर : वे सब हमारे चित्त में जमा हुई वृत्तियाँ हैं जो कि हमारे जन्म-जन्मांतरों से अंदर जमा हुई हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है, क्योंकि यह एक ऐसा भण्डार है जिसके अंदर से हमारे पास कभी भी, कुछ भी उठ आता है। इसलिए जब तक इस प्रकार हमारे भवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी घुस कर उपद्रव कर सकता है तब तक किसी प्रकार की शांति की और किसी विकासकार्य की तो कोई संभावना ही नहीं है। यह तो एक आम अनुभव है कि जब हम किसी समस्या के समाधान पर एकाग्र होने का प्रयास कर रहे होते हैं तब ऐसे-ऐसे विचार आदि उठ खड़े होते हैं जिनसे हमारा उस क्षण दूर-दूर तक भी कोई सरोकार नहीं होता। और हम स्वयं भी ऐसे अनचाहे आगंतुकों से परेशान हो जाते हैं। ये सब यांत्रिक वृत्तियाँ हैं जिन्हें हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण चित्त किसी भी गंभीर कार्य में एक बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। हालाँकि चित्त का अपना एक औचित्य है और हम यह नहीं कह सकते कि चूंकि वह बाधक बन जाता है इसलिए यदि संभव हो तो उसे किसी भी प्रकार निकाल कर बाहर कर देना चाहिये। परमात्मा का विधान इतना अनंतविध है कि वह हमारे किन्हीं भी मानसिक सूत्रों की पकड़ में नहीं आता। हमारा मन तो केवल एक सीधी रेखा खींचना जानता है जबकि भगवान् का सत्य तो इतना अनंत आयामी और अनंतविध है कि वह हमारे मन की किन्हीं भी रेखाओं की पकड़ में नहीं आ सकता। इसलिए चित्त हमें किसी भी एक रेखा या सूत्र को पकड़ कर आगे बढ़ने से रोक देता है। यदि वह हमें ऐसा करने से न रोकता तो हम किसी एक ही सूत्र को पकड़ कर निःशंक रूप से बेरोकटोक किसी एक ही दिशा में चल पड़ते और समग्र सत्य से बहुत दूर निकल जाते। इसलिए चित्त द्वारा बार-बार बाधा डाले जाने के कारण हमारे हृदय, बुद्धि आदि भागों में कुछ अधिक परिपक्वता आती है जिसके कारण हम कुछ आगे का मार्ग तय कर पाते हैं। और यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर चलती रहती है। चित्त की क्रिया के बाद भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एकांगी और असहिष्णु प्रकार के विचार भारी विनाश का कारण बने हैं। और यदि उसकी क्रिया न होती तब तो उस विनाश की कोई सीमा ही न होती। सारा इतिहास हमें इस बात के साक्ष्य देता है। कितनी-कितनी एकांगी विचारधाराएँ, कितने-कितने असहिष्णु धर्म, मत, संप्रदाय आदि हुए हैं जिन्होंने इतिहास में अपने काले धब्बे छोड़े हैं। इसलिए जिस प्रकार का हमारा गठन है उसमें आवश्यक ही है कि हमें अपनी किसी भी छोटी सी मानसिक संरचना को ही सब कुछ मान बैठने और उसे सभी पर थोपने के लिए स्वतंत्र नहीं होना चाहिये। इसीलिए चित्त कदम-कदम पर उसमें अपनी बाधा डालता है। हो सकता है कि व्यक्ति किसी एक प्रकार के सूत्र में ही अपने आप को बाँधना पसंद करे, परंतु जो परमात्मा स्वयं ही यह जीव बना है उसे ऐसी कोई भी कैद कैसे रास आ सकती है, वे इससे संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। इसीलिए जब वे हमारी संरचनाओं को तोड़ते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिक्रियाएँ करते हैं। अतः, इस विषय को इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है।
प्रश्न : गीता ने यहाँ यज्ञ का प्रतीक दिया है। यदि यह एक अध्यात्मपरक प्रतीक है तब फिर बाह्य यज्ञ-अनुष्ठान का क्या महत्त्व है?
उत्तर : यज्ञ के आंतरिक प्रतीक और उसके बाह्य अनुष्ठान के पीछे श्रीअरविन्द ने बहुत सी चीजें बतलाई हैं। विशद चर्चा के लिए तो यह एक बहुत ही विशाल क्षेत्र होगा परंतु कुछ बिंदुओं पर हम अवश्य ध्यान दे सकते हैं। जिस समय वेदों की रचना हुई वह एक अंतर्बोधात्मक काल था जब सामान्य मनुष्य मानसिक विकास में से नहीं गुजरा था। इसलिए जैसा कि श्रीअरविन्द बताते हैं कि ऋषियों ने परम सत्यों को वेदों में एक ऐसी भाषा में रखा जो प्रतीकात्मक थी और जिसे केवल कोई दीक्षित हो समझ सकता था जबकि किसी सामान्य सांसारिक व्यक्ति के लिए तो वह केवल बाह्य अनुष्ठान या फिर केवल बाहरी विषयों की ही चर्चा थी। यह तो एक बात हो गई। परंतु यदि केवल अध्यात्मपरक अर्थ ही एकमात्र चीज होती तब तो हमारी संस्कृति में वैदिक काल से ही बाह्य अनुष्ठान आदि को जो महत्त्व दिया जाता रहा है उसका कोई औचित्य ही नहीं होता। यहाँ तक कि वेदमंत्रों के उच्चारण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में लाखों लोग लगे थे ताकि एक मात्रा या स्वर तक में भी कोई त्रुटि न होने पाए। साथ ही पूरे के पूरे ग्रंथ केवल इन विषयों पर रखेंचे गए थे कि किस प्रकार बिल्कुल सटीक रूप से बाह्य अनुष्ठानों को किया जाए। बाह्य यज्ञ-कर्म के छोटे से छोटे ब्यौरों तक के लिए नियम-विधानों की रचना की गई और जो उस क्षेत्र में आगे जाना चाहता था उसे अनेकों वर्षों तक सतर्कतापूर्वक उन सब नियम-विधानों की शिक्षा दी जाती थी और यह सुनिश्चित किया जाता था कि वह कभी कोई त्रुटि न करने पाए। एक अर्थ में ज्ञानकाण्ड की बजाय कर्मकाण्ड पर अधिक बारीकी से ध्यान दिया जाता था। इसके पीछे एक बहुत ही गूढ़ कारण है। परमात्मा का सत्य इतना विशाल है कि वह हमारे ऊँचे से ऊँचे ज्ञान की पकड़ में नहीं आ सकता। यदि ज्ञान से ही वह सत्य पूर्णतया गम्य होता तब तो कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सारा कर्मकाण्ड अपने आप में भीतरी क्रिया का प्रतीक है। और जब हम कोई अनुष्ठान, कोई क्रिया आदि करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अतिरिक्त अन्य बहुत से भाग हैं जो जाने-अनजाने उस सत्य के संपर्क में आते हैं। साथ ही मंत्रोच्चार, यज्ञ-अनुष्ठान आदि सृष्टि-क्रिया की प्रतीकात्मक रूप से आवृत्ति करते हैं इसीलिए इन क्रियाओं से हमारी सत्ता का सत्य सुदृढ़ होता है। यही एक कारण है कि भले हम अनुष्ठानों को मानसिक रूप से न समझते हों और यहाँ तक कि उन्हें असभ्य या निरर्थक चीजें बताते हों फिर भी आज तक हमारे हर उपलक्ष्य पर किसी न किसी रूप में हम उनका अनुष्ठान अवश्य करते हैं। इन सबके पीछे एक बहुत ही गहरा सत्य निहित है जो हमारी बुद्धि के परे है इसलिए भले हम इन्हें मानसिक रूप से न समझकर इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हों, तब भी इन सभी क्रियाओं का अपना बड़ा भारी महत्त्व है और किसी न किसी रूप में ये हमें हमारी सत्ता के सत्य के साथ जोड़ देती हैं। वेदों की रचना किसी मानसिक उपकरण के द्वारा नहीं हुई। श्रीमाताजी अपने अनुभव के आधार पर बताती हैं कि किस प्रकार कोई भागवत् शक्ति हमारी भौतिक सत्ता तक को पूरी तरह से अधिग्रहीत कर सकती है और अपनी क्रिया संपन्न करा सकती है। परंपरागत भारतीय धारणा यही रही है कि सृष्टि के आरंभ में इसी प्रक्रिया से वेद ऋषियों के माध्यम से आए हैं। इसलिए उनमें जो सत्य निहित है वह आज भी उतना ही प्रयोजनीय है।
सारा ब्रह्माण्ड भी परमात्मा का एक प्रतीक है और जिस तत्त्व का यह प्रतीक है उसे हमारी चेतना के अनुसार प्रकट कर देता है। जिसकी चेतना जितनी विकसित होगी उतना ही तत्त्व उसके समक्ष प्रकट हो जाएगा। वेद परमात्मा की अभिव्यक्ति को समग्र रूप से प्रतीकात्मक भाषा में निरूपित करते हैं। इसलिए यदि कोई उन मंत्रों और उन ध्वनियों के माध्यम से उसमें निहित सत्य के साथ संपर्क साध सके तो उसे अपने मनोविज्ञान के पीछे स्थित विभिन्न शक्तियों का भी रहस्य प्रकट हो जाएगा और इस अस्तित्व की गुत्थी समझ में आ जाएगी और तब व्यक्ति अधिकाधिक आरोहण कर सकेगा। सत्य पर बुद्धि का एकाधिकार नहीं है। हमारी सत्ता का हर भाग अपने तरीके से उसे अभिव्यक्त करता है।
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
वेद्यं पवित्रमर्मोकार ऋक्साम यजुरेव च ।। १७।।
१७. मैं इस जगत् का पिता, माता, विधाता, पितामह (आदिस्रष्टा) हूँ, समस्त वेदों का ज्ञेय-विषय, पवित्र प्रणवाक्षर ॐ, और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेर हूँ।
----------------------------------------
*अ उ म - अ स्थूल और बाह्य जगत् का आत्मा 'विराट्' है, उ सूक्ष्म और आन्तर तुरीय है। आत्मा 'तैजस' है, म् गुह्य परमचेतन सर्वशक्तिमत्ता का आत्मा प्राज्ञ' है, ॐ परम,
- माण्डूक्य उपनिषद्
ज्योतिर्मय भगवान् स्वयं ही वेद हैं और वेदों के प्रतिपाद्य भी। वे ज्ञान और ज्ञेय दोनों ही हैं। ऋक्, यजुर्, साम - अर्थात् वह प्रकाशमय शब्द (मंत्र) जो बुद्धि को ज्ञान की किरणों से उद्बुद्ध कर देता है, कर्म के उचित विधान के लिए शक्तिमय शब्द (मंत्र), आत्मा की दिव्य कामना को चरितार्थ करने के लिए शान्त और सामंजस्यपूर्ण प्राप्ति का शब्द (मंत्र), - स्वयं ही ब्रह्म हैं, अधीश्वर हैं। दिव्य चेतना का मंत्र अपना प्रकटनकारी प्रकाश ले आता है, दिव्य शक्ति का मंत्र अपना कार्यसिद्धि का संकल्प ले आता है और दिव्य आनन्द का मंत्र समान ही रूप से अस्तित्व के आध्यात्मिक आनंद की परिपूर्णता ले आता है। समस्त शब्द और विचार महान् ॐ से ही पुष्पित हुए हैं - ॐ, महामंत्र, सनातन। ॐ, जो इन्द्रियगम्य पदार्थों के रूपों में व्यक्त है, जो सृजनशील आत्म-संकल्पन की उस सचेतन क्रीड़ा के रूप में व्यक्त है जिसके कि बाह्य रूप और पदार्थ रूपक हैं, जो पीछे अनन्त की आत्म-संयमित धीर अतिचेतन शक्ति में व्यक्त है, वह ॐ वस्तु और विचार, रूप और नाम का परम मूल, बीज और गर्भस्थान है, - वह स्वयं ही, पूर्ण रूप से, परम इन्द्रियातीत अथवा अग्राह्य है, मूल एकत्व है, वह कालातीत रहस्य है जो समस्त अभिव्यक्ति से ऊपर पुरुषोत्तम' में स्वतः-सिद्ध है। अतः यह यज्ञ एक साथ ही कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों है।
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ।। १८ ।।
१८. मैं पथ और लक्ष्य हूँ, मैं ही धारण करनेवाला, स्वामी, साक्षी, निवास-स्थान और आश्रय या शरण हूँ, मैं ही हितकारी मित्र, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ, मैं ही विश्रामस्थल और सभी का अविनाशी बीज हूँ।
तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ।। १९।।
१९. हे अर्जुन! मैं ऊष्णता प्रदान करता हूँ, मैं वृष्टि करता हूँ और उसे रोकता हूँ मैं ही अमरता हूँ और मृत्यु भी हूँ, और मैं ही सत् और असत् हूँ।
जो जीव इस प्रकार जानता, भक्ति करता और अपने सारे कर्म अपनी सत्ता के महत् आत्म-समर्पण में शाश्वत को अर्पण कर देता है उसके लिये ईश्वर सब कुछ है और सब कुछ ईश्वर है।.... जिसने अपने-आप को शाश्वत को समर्पित कर दिया है उसे जगत्, दैव और अनिश्चित घटना-चक्र डरा नहीं सकता और न इसका दुःख-संताप और अशुभ का पक्ष उसे व्याकुल ही कर सकता है। जो जीव इस प्रकार देखता है उसकी दृष्टि में ईश्वर ही मार्ग हैं और ईश्वर ही उसकी यात्रा का लक्ष्य हैं, एक ऐसा मार्ग जिसमें कोई आत्म-नाश नहीं होता और एक ऐसा लक्ष्य जिस तक उसके उचित रूप में मार्गदर्शित चरण निश्चय ही प्रतिक्षण पहुँच रहे हैं। वह ईश्वर को अपनी और सारी सत्ता का स्वामी, अपनी प्रकृति का धारक, प्रकृतिस्थ आत्मा का पति, उसका प्रेमी और पोषक, अपने सब विचारों और कर्मों का अंतःसाक्षी जानता है। ईश्वर ही उसका घर और देश है, उसकी सब वासना-कामनाओं का आश्रय-स्थान है, सब प्राणियों का घनिष्ठ तथा हितकारी ज्ञानी मित्र है। दृश्य जगत् के सारे रूपों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय उसकी दृष्टि और अनुभूति में वही एकमेव ईश्वर है जो अपने कालगत आत्माविर्भाव को उसकी निरंतर पुनरावर्तन की पद्धति से बाहर ले आता, बनाए रखता और फिर अपने अन्दर खींच लेता है। जो कुछ भी संसार में उत्पन्न होता और नष्ट होता दिखाई देता है उसका अविनश्वर बीज और मूल वही है और वही उस सबके अव्यक्त भाव का चिरंतन विश्रांति-स्थान है।.... वह सब जिसे हम 'सत्' कहते हैं, वही है और वह सब जिसे सभी 'असत्' मानते हैं, वह भी अनन्त के अन्दर छिपा हुआ है और उस परम अनिर्वचनीय की रहस्यमयी सत्ता का एक भाग है।
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्या स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ।। २० ।।
२०. तीनों वेदों को जाननेवाले, सोमपान करनेवाले, निष्पाप मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग को प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं; वे अपने पुण्यों के द्वारा इन्द्र के दिव्य लोकों को प्राप्त करके स्वर्ग में देवताओ के दिव्य भोगों को भोगते हैं।
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ।। २१ ।।
२१. वे उस पृथ्वी की अपेक्षा विशालतर सुखप्रद स्वर्गलोक को भोगकर अपने पुण्यों का फल क्षीण हो जाने पर मर्त्यलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वेदत्रय में प्रतिपादित सद्गुणों का आश्रय लेकर, अपनी कामना की तृत्ति को खोजते हुए वे जन्म-मरण के चक्र में गति करते हैं।
एकमात्र परम ज्ञान और भक्ति के अतिरिक्त कोई भी चीज, समा आत्म-निवेदन और समर्पण के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग हमें उन परम तक नहीं ले जाएँगे, जो कि सब कुछ हैं। अन्य धर्म, अन्य भजन-पूजन, अन्य ज्ञान, और साधन भी अवश्य ही अपने-अपने फल देनेवाले हैं, पर वे फल अल्पकालीन होते हैं और केवल दैवी प्रतीकों और रूपों के भोग देकर हो समाप्त हो जाते हैं।.... इसलिए प्राचीन समय के कर्मकाण्डी वेदत्रयी के बाह्यार्थ को सीखता, स्वयं को पापों से मुक्त कर पवित्र करता, देवताओं के संपर्कजनित सुधा का पान करता और यज्ञ-यागादि तथा पुण्य कर्मों द्वारा स्वर्ग के भोगों को पाने का प्रयत्न करता था। जगत् के परे किसी परम वस्तु में यह दृढ विश्वास और किसी दिव्यतर लोक का यह अन्वेषण मरणोपरान्त जीव को स्वर्ग के सुख-भोगों को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करता है, जिस पर उसकी श्रद्धा और उसकी चेष्टा केंद्रित थेः परन्तु वहाँ से जीव को फिर से मर्त्यलोक में आना पड़ता है, क्योंकि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पाया और उसे चरितार्थ नहीं किया गया होता है। अन्यत्र नहीं, इसी लोक में, परमोच्च ईश्वर को पाना होता है, जीव की अपूर्ण भौतिक मानव-प्रकृति में से उसकी दैवी प्रकृति का विकास करना होता है और ईश्वर, मनुष्य और जगत् के साथ एकत्व के द्वारा सत्ता के समग्र व्यापक सत्य को ढूँढ़ निकालना, उसे जीना और उससे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से विलक्षण और अद्भुत बनाना होता है। उसी से हमारे जन्म-मरण का लंबा चक्कर पूरा होकर हम परम फल पाने के अधिकारी बनते हैं; मानव जन्म के द्वारा जीव को यही सुअवसर प्रदान किया जाता है, जब तक इसका प्रयोजन पूर्ण नहीं होता तब तक जन्म-मरण का चक्कर रुक नहीं सकता।
जब तक इस पार्थिव जगत् में प्रभु का प्रयोजन पूर्ण नहीं होता तब तक जन्म-मरण रुक नहीं सकता। व्यक्ति चूँकि अपने अहं के दृष्टिकोण से देखता है इसलिए इस चक्कर से छूट निकलना चाहता है, परंतु जब स्वयं परम प्रभु ही जीव रूप से इस विकासक्रम में किसी प्रयोजन सिद्धि हेतु आए हैं तो वे अधूरे कार्य से संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। अहमात्मक चेतना को यह विश्व-प्रपंच जैसा लगता है वैसा अवश्य ही परम प्रभु को बिल्कुल भी नहीं लगता, इसलिए उन्हें इसमें से किसी प्रकार निकल भागने की कोई अधीरता नहीं है।
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।। २२ ।।
२२. जो मनुष्य अनन्य रूप से मुझे अपने चिंतन का संपूर्ण विषय बनाकर मेरी उपासना करते हैं, मेरे साथ सदा योगयुक्त रहनेवाले उन मनुष्यों का मैं स्वतः ही सर्वविध कल्याण करता हूँ और उनके सभी अंतर्बाह्य योग और क्षेम को मैं पूर्ण करता हूँ।
ईश्वर-प्रेमी जगत्-व्यवस्था में हमारे जन्म के इस परम प्रयोजन की ओर अनन्य प्रेम और भक्ति के द्वारा सतत् आगे बढ़ता रहता है, जिसके द्वारा वह परमेश्वर और जगदीश्वर को न कि अपनी अहंपरक पार्थिव तुष्टि को और न ही स्वर्गीय लोकों के भोगों को अपने जीवन का, अपने चिंतन और अपने दर्शन का संपूर्ण लक्ष्य बना लेता है। अन्य कुछ नहीं, केवल भगवान् को ही देखना, प्रतिक्षण उन्हीं के साथ एकत्व में रहना, सब प्राणियों में उन्हीं से प्रेम करना और सब पदार्थों में उन्हीं का आनन्द लेना - यही उसके आध्यात्मिक जीवन की संपूर्ण दशा होती है। उसका भगवद्दर्शन उसे जीवन से विच्छिन्न नहीं करता, और न ही जीवन की परिपूर्णता का कोई अंश वह खोता है; क्योंकि भगवान् स्वयं उसका सहज ही सर्वविध कल्याण साधित करने वाले और उसका अंतर्बाह्य सारा योग और क्षेम वहन करने वाले बन जाते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्वर्ग-सुख और पार्थिव सुख तो उसकी निधियों की केवल एक छोटी छायामात्र है; क्योंकि ज्यों-ज्यों वह भगवान् में विकसित होता जाता है, त्यों-त्यों भगवान् भी अपनी अनन्त सत्ता की सारी ज्योति, शक्ति और आनन्द के साथ उसके ऊपर प्रवाहित होने लगते हैं।
अधिकांशतः इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि भगवान् व्यक्ति के बाहरी साधनों की आपूर्ति करते हैं, उसके खाने-पीने की, रहने-सहने
आदि की व्यवस्था करते हैं। परंतु क्या हम बुद्धि से वास्तव में जानते हैं कि हमारे योग के निर्वहन के लिए क्या-क्या आवश्यक है? यदि हमारे योग के लिए हमें कष्टों की, थपेड़ों की, अपयश आदि की आवश्यकता हो तो भगवान् हमारे लिए बेझिझक उनकी व्यवस्था कर देंगे क्योंकि वे बड़े ही कृपालु हैं। परंतु इन सब चीजों को हम योगक्षेम नहीं मानते। जिस भी चीज की हमारे योग के लिए आवश्यकता है भगवान् उस सब की पूर्ति अवश्य करते हैं, परंतु हमें किस चीज की वास्तव में आवश्यकता है यह निर्णय हमारे अनुसार नहीं अपितु दिव्य विधान के अनुसार होता है। अन्यथा इस बात का व्यक्ति दुरुपयोग करते हुए सोच सकता है कि उसे कोई भी पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं।
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ।। २३ ।।
२३. हे कुन्ती पुत्र! जो भक्त श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं के लिये यज्ञ करते हैं वे भी मेरे ही लिये यज्ञ करते हैं; किंतु उनका यह यज्ञ यथार्थ विधि के अनुसार नहीं होता।
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात श्वयवन्ति ते ।। २४।।
२४. स्वयं मैं ही हूँ जो समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, किन्तु वे मुझे यथार्थ तत्त्वों में नहीं जानते और इस कारण च्युत हो जाते हैं।
सभी सच्चे धार्मिक विश्वास और अभ्यास अथवा साधना यथार्थ में एकमेव परम और वैश्विक ईश्वर की खोज हैं; क्योंकि वे सदा ही मनुष्य के यज्ञ और तप के एकमात्र स्वामी हैं और उसके प्रयास और उसकी अभीप्सा के अनन्त भोक्ता हैं। पूजा-अर्चना का रूप चाहे कितना ही छोटा या नीचा क्यों न हो, परमेश्वर की कल्पना चाहे कितनी ही सीमित क्यों न हो, आत्मदान, श्रद्धा-विश्वास, अपने ही अहंकार की पूजा के आवरण और जड़-प्रकृति के प्रतिबंधों के परे पहुँचने का प्रयास चाहे कितना ही संकुचित क्यों न हो, फिर भी यह मनुष्य की आत्मा और सर्वात्मा के बीच एक संपर्क-सूत्र बन जाता है और प्रत्युत्तर मिलता ही है। तथापि यह प्रत्युत्तर, आराधना और अर्पण से मिलनेवाला प्रतिफल ज्ञान, श्रद्धा और कर्म के अनुसार ही होता है, इनकी मर्यादाओं का वह अतिक्रम नहीं कर सकता, और इसलिए उस महत्तर ईश्वर-ज्ञान की दृष्टि से – केवल वही जो सत्ता और भूतभाव के समग्र सत्य को प्रदान कर सकता है - यह निम्न कोटि का आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग के सच्चे और परम विधान के अनुसार नहीं होता। यह आत्मोत्सर्ग या यज्ञ परम् पुरुष परमेश्वर के समग्र स्वरूप और उनके आत्माविर्भाव के सच्चे तत्त्वों के ज्ञान पर प्रतिष्ठित नहीं होता, अपितु अपने-आप को बाह्य और आंशिक रूपों से ही संलग्न कर लेता है, न माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन । अतः इसके द्वारा होनेवाला आत्मदान (यज्ञ) भी अपने लक्ष्य में सीमित, हेतु में भारी रूप से अहंभावयुक्त, कर्म और दान-क्रिया में आंशिक और अशुद्ध या अविधिपूर्वक होता है, यजन्ति अविधिपूर्वकम्।
यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ।। २५।।
२५. जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करनेवाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों के लिये यज्ञ करनेवाले भूतों को प्राप्त होते हैं; किन्तु मेरे उपासक मुझे प्राप्त होते हैं।
भगवान् का समग्र दर्शन एक समग्र सचेतन आत्म-समर्पण द्वारा ही साधित होता है; शेष सब तो उन चीजों को प्राप्त करता है जो अपूर्ण और आंशिक हैं और उसे उन्हें प्राप्त करने के बाद वहाँ से पुनः पतित होकर महत्तर खोज और विशालतर ईश्वर-अनुभव में अपने-आप को अधिक विशाल बनाने के लिए लौट आना पड़ता है। परन्तु परम् पुरुष और विश्वात्मपुरुष को ही अनन्य रूप से और संपूर्ण रूप से प्राप्त करने का यत्न करना उस सब ज्ञान और फल को प्राप्त होना है जिसे अन्य मार्ग प्राप्त कराते हैं जब कि यहाँ साधक किसी एक ही पहलू से सीमित नहीं रहता, तथा वह भगवान् के सत्य को सभी पहलुओं में अनुभव करता है। इस प्रकार का यत्न परम् पुरुषोत्तम की ओर आगे बढ़ता हुआ भगवद्-सत्ता के सभी रूपों को अंतर्निहित करता है।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ।। २६।।
२६. एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, जल, जो कुछ भी व्यक्ति भक्तिपूर्वक मुझे अर्पण करता है, उस यत्नशील आत्मा के द्वारा वह प्रेम-भक्ति युक्त भेंट मुझे स्वीकार है।
.....केवल कोई समर्पित बाहरी भेंट ही नहीं है जो इस प्रकार प्रेम और भक्तिपूर्वक दी जा सकती है, अपितु हमारे सब विचार, हमारी सभी भावनाएँ और संवेदन, हमारी सब बाह्य क्रियाएँ और उनके रूप एवं विषय भी शाश्वत के प्रति ऐसी भेंट हो सकते हैं। यह सच है कि एक विशिष्ट कार्य का या का के किसी विशेष रूप का अपना महत्त्व होता है. यहाँ तक कि अत्यधिक महत्त्व होता है, परंतु कार्य में निहित भाव ही है जो मुख्य तत्त्व है; वह भाव ही जिसका कि वह कार्य प्रतीक या मूर्त अभिव्यक्ति होता है, इस कार्य को इसका संपूर्ण मूल्य और इसका औचित्यपूर्ण महत्त्व प्रदान करता है। अथवा प्रेम और पूजा के पूर्ण कर्म में तीन होते हैं जो एक ही अखंड समग्र की अभिव्यक्तियाँ होते हैं, - कर्म में भगवान की क्रियात्मक पूजा, कर्म के बाह्य रूप में किसी दिव्य दर्शन एवं अन्वेषण को या भगवान् के साथ किसी संबंध को प्रकट करने वाला पूजा-प्रतीक, अ तीसरा, हृदय, अंतरात्मा और आत्मा में एकत्व या एकत्वानुभूति के लिये आंतरिक आराधन एवं उत्कंठा। इस तरीके से ही जीवन को पूजा में परिवर्तित किया जा सकता है, - इसके पीछे परात्पर तथा सार्वभौम प्रेम का भाव और एकत्व की उत्कण्ठा एवं एकत्व के बोध को प्रतिष्ठित करके; प्रत्येक क्रिया को एक प्रतीक बनाकर, ईश्वरोन्मुख भाव की या भगवान् के साथ सम्बन्ध की अभिव्यक्ति बनाकर; जो कुछ हम करते हैं - मन की समझ, प्राण के आज्ञापालन और हृदय के समर्पण - इस सब को पूजाकार्य में तथा आत्मा के अन्तर्मिलन में परिवर्तित करके।
यह पूर्ण आत्मोत्सर्ग, यह एकनिष्ठ समर्पण ही वह भक्ति है जिसे गीता अपने समन्वय का शीर्ष बनाती है। सारा कर्म और प्रयास इस भक्ति के द्वारा उस परम-पुरुष जगदीश्वर के प्रति एक भेंट के रूप में परिणत हो जाता है।
______________________________
* कर्म का एक निरा भौतिक रूप होता है, पूजा-पद्धतियों के उन रूपों के जैसा जिनमें कोई विशेष भाव-भंगिमा, कोई विशेष क्रिया आत्मोत्सर्ग के भाव को अभिव्यत करने के उद्देश्य से प्रयुक्त होती है। वह विशुद्ध रूप में भौतिक होता है, उदाहरणार्थ, धूपबत्ती जलाना, पूजा-सामग्री को सजाकर रखना, यहाँ तक कि मंदिर की देख-भाल करना, मूर्ति को सजाना आदि, इस प्रकार की सब विशुद्ध भौतिक क्रियाएँ।
दूसरा भाग होता है एक प्रकार का मानसिक आत्मोत्सर्ग-भाव जो किये जाने वाले कर्म को एक प्रतीक बना देता है। तब मनुष्य धूपबत्ती मात्र जलाने से ही संतुष्ट नहीं हो जाता, अपितु धूपबत्ती जलाते समय वह इस क्रिया को प्रतीकात्मक बना देता है जो, उदाहरणार्थ, शरीर में जलती हुई अभीप्सा का अथवा आत्म-विलोपन के लिये, अग्नि के शुद्धिकरण के लिये किये गये आत्म-दान का प्रतीक होता है। अर्थात्, पहले तो बाह्य क्रिया होती है, फिर इस क्रिया में निहित प्रतीक, और जो कुछ किया जाता है उसका प्रतीकात्मक ज्ञान।
और अंत में, इन दोनों के पीछे, एकत्व की अभीप्सा होती है; कि यह सब, ये क्रियाएँ तथा इनके साथ वह प्रतीकात्मक स्वरूप जो तुम इन्हें प्रदान करते हो, ये सब भगवान् के क्रमशः अधिकाधिक समीप जाने तथा अपने-आप को उनके साथ युक्त होने के उपयुक्त बनाने के साधनमात्र बन सकते हैं।
क्रिया को पूर्ण बनाने के लिए ये तीनों चीजें अवश्य विद्यमान होनी चाहिए: अर्थात कोई शुद्ध भौतिक वस्तु, कोई मानसिक वस्तु, और कोई आंतरात्मिक वस्तु, चैत्य अभीप्सा यदि तीनों में से बाकी दोनों के बिना कोई एक वस्तु हो तो वह क्रिया अपूर्ण होगी। सामान्यतया कदाचित् ही ये तीनों सचेतन रूप में संयुक्त होती हैं। यही बात विलक्षण मैं, वाई एवं आत्म-दान से उस क्रिया में भाग लेती है।
जब व्यक्ति भगवान् से प्रेम करता है तब उसकी क्रिया उस प्रेम के अनुसार होती है न कि उसके अपने अहं के अनुसार। हालाँकि चेतना के इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतया बहुत लंबा समय लगता है परंतु इस परिवर्तन के होने के बाद इसकी क्रिया सबसे तेज और सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। जब हमारी बुद्धि में किसी कार्य को करने का विचार उठता है तब उसमें उसे चरितार्थ कर पाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होती इसलिए उसे चरितार्थ करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वहीं यदि हमारा हृदय किसी चीज के लिए द्रवित हो उठता है तब व्यक्ति को उसकी ओर चलने से कोई नहीं रोक सकता। बिना हृदय के द्रवित हुए किसी प्रकार का समर्पण कभी नहीं हो सकता। इस संदर्भ में दिलीप कुमार रॉय द्वारा पूछे एक प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्णप्रेम का बड़ा ही मार्मिक उत्तर है।
दिलीप कुमार रॉय ने पूछा, "एक और प्रश्न है जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ यदि तुम बुरा न मानो तो.... तुम देखो, इस बात पर मुझे कभी-कभी संशय हुआ है कि क्या जिस विजय की तुम बात करते हो वह केवल घोर परिश्रम करके अपनी स्वेच्छा को संकल्प-शक्ति से बदल देने मात्र से साधित नहीं हो सकती? क्या तुम्हें प्रेम पर आग्रह करने की आवश्यकता है? ....मेरा मतलब है कि यदि इस प्रकार की परिणति की निष्ठापूर्वक इच्छा रखी जाए, तो क्या प्रेम का समाविष्ट होना या उसका हस्तक्षेप आवश्यक है, और ऐसी स्थिति में एक अपरिहार्य प्रश्न उठता है: प्रेम का आह्वान किया कैसे जाए? तुम इच्छा पर तो अधिकार रख सकते हो, परंतु प्रेम पर नहीं, क्या कर सकते हो? प्रेम तो जब आता है तभी आता है - क्या हम सभी नहीं जानते?"
उन्होंने मुझ पर एक व्यंग्यमिश्रित दृष्टि से देखा और फिर दृढ़तापूर्वक अपना सिर हिलाया।
"नहीं दिलीप, इससे काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है और क्यों प्रेम के आह्वान को तुम अव्यावहारिक बताकर इसे टालकर इससे बचना चाहते हो, जी चुराना चाहते हो। परंतु वहाँ तुम गलत हो, क्योंकि तुम एकमात्र अपनी संकल्प-शक्ति के सहारे ही अपनी स्वेच्छा को कम नहीं कर सकते। जब तक कि प्रेम का समर्थन प्राप्त नहीं होता तब तक यह नहीं किया जा सकता। क्योंकि केवल प्रेम ही समर्पण को एक हर्ष का विषय बना सकता है। यदि प्रेम न हो तो अहंकार कभी भी समर्पण के निरंतर कष्ट से गुजर नहीं सकता। केवल प्रेम का ऊर्जा-स्रोत (पावर-हाउस) ही वह विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम है जिसके द्वारा योग की चक्की या कारखाने को चलाया जा सकता है। ...सच्चे प्रेम का सार-रूप सामने नहीं आ सकता जब तक कि तुमने अहं के बाहरी खोल को तोड़ न दिया हो, अर्थात् तुम्हारी स्व-इच्छा को। यहाँ एकमात्र कठिनाई यह है कि जब तक प्रेम अग्रणी नहीं होता - या फिर जैसा कि तुम्हारे गुरुदेव कहते हैं, चैत्य पुरुष सामने नहीं आ जाता - तब तक अहं का कठोर खोल बिल्कुल तोड़ा ही नहीं जा सकता और वहाँ फिर तुम दुष्वक्र में फँस जाते हो, क्योंकि जब तक अहं की दीवारों को गिरा नहीं दिया जाता तब तक प्रेम भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु वास्तव में ही ये आत्मा की गहनतम पहेलियाँ हैं और तब तक असमाधेय ही बनी रहेंगी जब तक कि इन्हें शुद्ध-बुद्धि के प्रकाश द्वारा पुनः अनावृत नहीं कर दिया जाता..." (योगी श्रीकृष्णप्रेम, श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट, पृष्ठ ८८)
पत्र, पुष्प, फल आदि भेंट करने से वास्तव में अर्थ है कि अपनी से छोटी चीज को अर्पित कर देना। और भगवान् कहते हैं कि वे तो छोटी छोटी से छोटी चीज को भी स्वीकार कर लेते हैं। आरंभ में ही ऐसा संभव नहीं होता कि व्यक्ति अपने सभी भाव अर्पित कर पाए। कुछ भावों को व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक सहजता से अर्पित कर सकता है परंतु कुछ ऐसे भाव हैं जिनमें व्यक्ति गहराई तक आसक्त रहता है और उन्हें अर्पित करना उसके लिए अधिक मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, साधना के लिए कदम बढ़ा लेने पर भी व्यक्ति की अपने परिवार में, या परिवार के किसी सदस्य में, किसी छोटे बच्चे में या फिर अन्य किसी वस्तु में गहरी आसक्ति बनी रह सकती है जिसे छोड़ने में उसे बहुत कष्ट का अनुभव होता है। परंतु यदि मन में परमात्मा के प्रति थोड़ा-बहुत भी संकल्प आ गया है तो उसके सहारे यज्ञ का आरंभ हो जाता है और धीरे-धीरे वह अन्य भागा को भी यज्ञ में सम्मिलित कर लेता है। कहने का अर्थ है कि छोटे से छोटा काम भी यदि व्यक्ति अपने अहं की बजाय परमात्मा के निमित्त करता है तो उसका बड़ा भारी महत्त्व है। और वास्तव में तो आरंभ होता ही इसी प्रकार है, क्योंकि आरंभ में ही व्यक्ति सभी कुछ समर्पित कर दे ऐसा संभव नहीं होता। आरंभ में तो कोई केंद्रीय संकल्प जागृत होता है जो व्यक्ति को परमात्मा की ओर मोड़ देता है। परंतु व्यावहारिक जीवन में उस संकल्प को चरितार्थ करना ही तो साधना है। और यह व्यक्ति की अभीप्सा और उसके संकल्प की तीव्रता पर निर्भर करता है कि साधना पथ पर वह किस गति से आगे बढ़ता है। इसलिए जब भगवान् पत्र, पुष्प आदि जैसी छोटी सी भेंट की बात करते हैं तब वह इस बात का प्रतीक है कि भक्तिपूर्वक छोटी से छोटी भेंट का भी हमें बड़ा भारी प्रतिफल प्राप्त होता है। हमारे अंदर ऐसे-ऐसे भाग होते हैं जो हमारे साधना पथ पर बहुत आगे जाने पर भी अपनी स्व-इच्छा बनाए रख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे अंदर ऐसे अनगिनत छोटे-छोटे हिस्से छिपे होते हैं जिन्हें हमारे समर्पण से कोई सरोकार नहीं होता। हमारी बाह्य सत्ता के इस प्रकार के गठन के कारण ही कोई भी छोटी से छोटी सच्ची भेंट भी इतनी महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि वास्तव में ये भाग भगवान् को कुछ भी भेंट करना चाहते ही नहीं। इसीलिए जो कोई जिस किसी भी भाव से भगवान् की ओर मुड़ता है, चाहे तकलीफ के कारण हो, किसी स्वार्थपूर्ति के लिए हो या फिर किसी जिज्ञासावश हो, गीता सभी को ही श्रेष्ठ बताती है क्योंकि वे जिस किसी भी कारण से हो, पर भगवान् की ओर मुड़ तो जाते हैं, और वही सबसे महत्त्वपूर्ण बात है।
ज्यों-ज्यों व्यक्ति परमात्मा की ओर बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों उसमें अधिकाधिक समता आती जाएगी क्योंकि तब सभी चीजों के पीछे उसे प्रभु की क्रिया गोचर होने लगेगी। और जब सभी चीजों के पीछे उन्हीं का हाथ दिखेगा तब कौनसी चीज है जिससे कि व्यक्ति विचलित हो पाए। पहले यह समता उन चीजों के विषय में होगी जिनसे व्यक्ति अधिक विचलित नहीं होता। धीरे-धीरे यह समता उन भागों में भी आती जाएगी जिनमें हम अतिशय रूप से आसक्त रहते हैं। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर ज्यों-ज्यों भगवान् के प्रति प्रेम का यह भाव बढ़ता जाता है त्यों-त्यों दुनिया के विषय में उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदलता जाता है। यदि यह प्रेम का भाव न आए तो व्यक्ति केवल अपने अहं की, मन, प्राण और शरीर की क्षुद्र संतुष्टियों की पूर्ति में ही लगा रहता है। श्री अरविन्द भक्ति के इसी तत्त्व को विकसित करेंगे।
प्रश्न : यहाँ पाद-टिप्पणी में उल्लेख है कि कर्म का एक निरा भौतिक रूप होता है और दूसरा भाग होता है एक प्रकार का मानसिक आत्मोत्सर्ग-भाव जो किये जाने वाले कर्म को एक प्रतीक बना देता है। तो इसका क्या अर्थ है कि वह कर्म को एक प्रतीक बना देता है?
उत्तर : किसी भी कर्म को पूर्ण बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है : शुद्ध भौतिक कर्म, उसके पीछे कोई मानसिक भाव, और उसके साथ ही एकत्व के लिए चैत्य अभीप्सा। सामान्यतया हम सुनते हैं कि वास्तव में तो कर्म के पीछे के भाव का महत्त्व है, बाड़ा पूजा तो बड़ी अधम चीज है। जब दिलीप कुमार रॉय ने स्वामी ब्रह्मानंद द्वारा अपनी पुस्तक में उद्धृत किये एक श्लोक का श्रीकृष्णप्रेम के सामने उल्लेख करते हुए कहा कि, 'उच्चतम पूजा उस चेतना या भाव में स्थित होती है जिसमें तुम प्रभु को सभी चीजों में देखते हो। उससे निचले दर्जे का है ध्यान। उससे भी निम्नंतर है स्तुतिगान या नाम जप और सबसे ही निम्न है बाह्य पूजा, औपचारिक सेवा', तब श्रीकृष्णप्रेम ने तीव्र रूप से इस बात पर अपनी आपत्ति जताई और कहा कि, "इस प्रकार के उद्धरण बहुत भारी क्षति पहुँचाते हैं यदि उनका अर्थ अपनी संपूर्णता से अलग करके खंड-खंड में आँका जाता है और फिर उन्हें सत्य की दीपशिखाओं में विकसित कर दिया जाता है जो प्रकाशित करने की बजाय छाया अधिक डालती हैं।" (योगी श्रीकृष्णप्रेम, पृष्ठ ७८)
श्रीकृष्णप्रेम ने तो अक्षरशः वैष्णव तंत्र का पालन किया था और उसके सभी बाहरी निषेधाज्ञाओं का नैष्ठिक रूप से पालन किया था। और अपने जीवन के द्वारा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार एक पूर्ण कर्म, जिसमें बाहरी क्रिया, उसके पीछे का भाव और चैत्य अभीप्सा साथ मिलने पर भगवान् की जीवंत उपस्थिति ले आता है। अतः किसी भी कर्म को पूर्ण बनाने के लिए उसमें तीन चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहला है पूजा का एक भौतिक रूप जैसे कि शिवजी को जल या दूध अर्पित करना, या फिर धूपबत्ती जलाना या अन्य कुछ, उसके बाद, उस बाह्य कर्म के पीछे यह मानसिक भाव या कल्पना कि किस प्रकार भगवान् को यह दूध अर्पण करना आत्मा को पुष्ट करना है। और अंत में यह भाव कि जो कुछ पूजा हम कर रहे हैं वह हमें परमात्मा के साथ युक्त कर दे। इन तीनों में से कोई भी एक छूट जाये तो कर्म पूर्ण नहीं हो सकता।
श्रीअरविन्द ने अपने योग में भौतिक कर्म को अत्यावश्यक बताया है क्योंकि इसी के द्वारा हमारी भौतिक चेतना को भगवान् के लिए कार्य करने का आनंद और उनके संपर्क में आने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही भौतिक कर्म करने से व्यक्ति का सही संतुलन बना रहता है। यदि व्यक्ति भौतिक कर्म न करे और केवल ध्यान आदि में ही लगा रहे तो अधिकांशतः व्यक्ति का संतुलन बिगड़ने की आशंका रहती है। इसकी बहुत कुछ संभावना रहती है कि व्यक्ति स्वयं अपने ही किन्हीं मनोनिर्मित जगतों में निवास करने लगे जिनसे निकल पाना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाय। परमहंस योगानन्द जी की शिष्या दया माता भी कर्मयोग को अत्यंत महत्त्व प्रदान करती थीं। वे कहती थीं कि आध्यात्मिक पथ पर संतुलन बनाए रखने के लिए भौतिक कर्म करना अत्यावश्यक है। श्रीअरविन्द भी कहते हैं कि भौतिक कर्म के बिना भौतिक रूपांतर का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।
भारतीय संस्कृति ने सदा ही भगवान् के प्रति निवेदित कर्म को महत्त्व दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने कर्म में आनन्द का अनुभव होता था और चूंकि प्रत्येक को अपने कर्म में अत्यंत आनंद आता था इसीलिए भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता के उदाहरण आज भी प्रचलित हैं। अब यदि कर्म अपने आप में कोई बाध्यता या बोझ न रहकर आनन्द का साधन बन जाए, अपनी आत्म-अभिव्यक्ति का साधन बन जाए, परमात्मा से मिलने का, उनसे संपर्क साधने का माध्यम बन जाए तब तो कोई भी व्यक्ति कर्म किये बिना कैसे रह सकता है। इसी कारण ऐसा कौनसा क्षेत्र रहा है जिसमें भारत ने विपुल रूप से और सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता की रचना न की हो। वहीं यदि व्यक्ति को कर्म बोझ लगने लगे तब तो वह स्वयं भी उसे करने से पीड़ित रहेगा, अपने सहयोगियों को और सहकर्मियों को पीड़ित करेगा और उसका कर्म भी गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक से अधिक केवल कोई औसत दर्जे का ही होगा। परंतु जब भावना को भगवान् की ओर मोड़ दिया जाता है और कर्म में आनन्द की अनुभूति होने लगती है तब तो जिस मात्रा और गुणवत्ता की रचना की जाती है वह तो अतुलनीय होती है। आज भी विध्वंस की अनेकों शताब्दियाँ बीत जाने के बाद भी भारतीय रचनाओं का जो कुछ भी अंश हमारे पास शेष बचा रहता है उसका भी कोई सानी नहीं है और उसे भी हम आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं कि वह संभव कैये हो पाया।
"सबसे पहले गीता ने कर्मयोग की चर्चा की, उसके बाद ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बताया, अब यहाँ गीता उनमें भक्ति तत्त्व को जोड़ रही है। तात्पर्य यह है कि समग्र रूप से कर्म तभी होंगे जब तीनों चीजें सम्मिलित हो। हमारे कर्मों के पीछे भाव और आत्मा हो तो कर्म भक्ति प्रधान हो जायेंगे और हमारे उत्थान का एक सशक्त साधन बन जाएँगे और ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे हम परमात्मा से न जोड़ सकें।
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासियत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ।। २७।।
२७. हे कौन्तेय! तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोग करता है, जो कुछ यह (उत्सर्ग) करता है, जो कुछ दान करता है, तपस्या की ऊर्जा, आत्मा का संकल्प अथवा प्रयास जो तू करता है, उसे मेरे प्रति एक भेंट बना दे।
यह समग्र भक्ति का स्वरूप है। इससे पिछले श्लोक में गीता भौतिक चीजों को भेंट करने की बात कहती है। अब गीता इन सब प्राणिक, मानसिक ऊर्जा, संकल्प आदि को भी भेंट करने की बात कर रही है। इस प्रकार गीता हमारी सत्ता की सभी क्रियाओं, सभी मनोवैज्ञानिक शक्तियों, मानसिक, प्राणिक संकल्पों, ऊर्जाओं आदि में भी भक्ति को प्रविष्ट कर रही है। इसी बात का श्रीअरविन्द यहाँ विवेचन कर रहे हैं।
यहाँ छोटी-से-छोटी चीज, जीवन की सामान्य-से-सामान्य घटना, हम जो कुछ हैं या हमारे पास जो कुछ है उसका किंचित्मात्र भी दान, छोटे-से-छोटा कर्म दिव्य महत्त्व प्राप्त कर लेता है और भगवान् के लिए ग्रहण कर सकने योग्य भेंट बन जाता है जो इसे ईश्वर-प्रेमी की आत्मा और उसके जीवन पर अधिकार पाने का एक माध्यम बना लेते हैं।
यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। हम जो कुछ हैं और जो कुछ हमारे पास है उसका किंचित् मात्र भी दान एक दिव्य महत्त्व प्राप्त कर लेता है। परन्तु यहाँ भगवान् हमसे हम जो कुछ भी हैं अथवा जो कुछ भी हमारे पास है, उस सब की माँग कर रहे हैं। वर्तमान में तो हम अपना सर्वस्व अपने अहंकार की सेवा में अर्पित करते हैं जहाँ कि अहंकार राजा के रूप में अपने आसन पर विराजमान है और मिथ्यात्व उसकी रानी के रूप में उसके साथ विराजमान है। वर्तमान में तो अहं का साम्राज्य इतना फैला है कि हम यह मानने को भी वास्तव में तैयार नहीं होते कि हम अहं के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में यदि हम इस चीज के लिए आश्वस्त हो जाएँ कि हम अहं से मुक्त हो गए हैं तब तो उससे मुक्त होने की तो हमारी कोई संभावना भी नहीं रहती। इसलिए व्यक्ति को यह मानकर चलना चाहिये कि अहं की पाश में तो वह अवश्य ही है, ऐसे में करने का काम केवल यह है कि यह ढूँढ़े कि वह पाश कहाँ है और वहाँ उसे कुछ ढीला करने का प्रयास करे। आम तौर पर समाज में हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो परोपकारिता के कार्यों में अपना समय, अपना धन आदि लगाते हैं, जैसे कि गरीबों की सेवा करना, गोशाला में दान करना, पीड़ितों के इलाज आदि के लिए धन देना, आदि-आदि। इन सब कार्यों में व्यक्ति को सच में ऐसा प्रतीत होता है कि वह तो अहं से मुक्त होकर सबकी निःस्वार्थ रूप से सेवा कर रहा है और गीता का कर्मयोग ही कर रहा है। इस विषय पर श्रीमाताजी के वचन बहुत ही मार्मिक और उद्बोधक हैं। वे कहती हैं,
"... यदि तुम मानवजाति की सहायता करना चाहते हो तो एक ही काम करने लायक है। अपने-आपको, जितना संभव हो, पूरी तरह से भगवान् के अर्पण कर दो। यही समाधान है। ...
...तुम क्या हो? तुम बस जरा सी चेतना और जरा से भौतिक पदार्थ के प्रतिनिधि हो। बस, उसी को तुम 'मैं' कहते हो। यदि तुम मानवजाति की, संसार या विश्व की सेवा करना चाहते हो तो करने लायक यही है कि उस छोटे से टुकड़े को पूरी तरह भगवान् को अर्पण कर दो। ... जो कुछ तुम्हारा है उसे दे दो। उसे पूरी तरह, समग्र रूप में भगवान् को दे दो...इससे अच्छा कोई समाधान नहीं है। तुम मानवजाति की सहायता कैसे करना चाहते हो? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिये ।...
...यदि यही लोग जो विद्यालयों के लिये पैसा देने को तैयार होते हैं, उनसे कहा जाय कि कोई भगवान् का काम है जिसे भगवान् ने अमुक तरीके से करने का निश्चय किया है, और यदि उन्हें विश्वास भी हो कि यह सचमुच भगवान् का कार्य है, तो भी वे कुछ देने से इंकार करते हैं, क्योंकि यह सर्वसम्मत परोपकार का काम नहीं है - यह करके कुछ अच्छा करने का संतोष नहीं होता! मैं एक विनोदप्रिय व्यक्ति को जानती थी जो कहा करता था : 'भगवान् का राज्य बहुत जल्दी नहीं आयेगा क्योंकि तब इन बेचारे परोपकारियों के लिये क्या बचा रहेगा? यदि मानवजाति दुःख न भोगती रहे तो बेचारे परोपकारी लोग बेकार हो जायेंगे।' इसमें से निकलना मुश्किल है। फिर भी यह तथ्य है कि दुनिया इस स्थिति में से तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक कि वह अपने-आप को भगवान् को न सौंप दे। सभी सद्गुण – तुम उनकी चाहे जितनी महिमा गाओ तुम्हारी आत्म-संतुष्टि को, यानी, अहं को बढ़ाते हैं। वे तुम्हें सचमुच भगवान् के बारे में सचेतन होने में सहायता नहीं देते। दुनिया के बुद्धिमान् और उदार लोगों को बदलना सबसे कठिन होता है। वे अपने जीवन से बहुत संतुष्ट होते हैं। एक गरीब व्यक्ति जिसने जीवन में सब प्रकार की बेवकूफियाँ की हैं तुरंत दुःखी हो उठता है और कहता है : मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम जो बनाना चाहो बना लो।" यह व्यक्ति ज्यादा ठीक है और यह भगवान् के, उस व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक निकट है जो बुद्धिमान् है तथा अपनी बुद्धिमत्ता और गर्व से भरा है। यह अपने-आप को वैसा ही देखता है जैसा कि वह है।" (CWM 5, 12-14)
अब प्रश्न यह उठता है कि यह भेंट हो किस प्रकार से? क्योंकि गीता में आरंभ से ही हमने देखा है कि जो प्रसंग हमें सतही भी प्रतीत होते हैं वे भी अपने वास्तविक स्वरूप में अत्यंत गंभीर होते हैं। इसलिए गीता जिस भेंट की बात कर रही है वह यदि कोई सतही प्रकार की होती तब तो सभी अपने-अपने तरीके से भेंट कर ही रहे हैं। और फिर श्रीअरविन्द की टीका से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जिस स्थिति की गीता बात कर रही है वह तो एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था है जहाँ तक सहज ही नहीं पहुँचा जा सकता।
श्रीअरविन्द और श्रीमाताजी के आलोक में यदि हम इसे देखें तो व्यावहारिक रूप से इस भेंट की कहीं किसी भाग में थोड़ी शुरुआत होती है। और फिर वह धीरे-धीरे हमारी सत्ता को, हमारे सारे क्रिया-कलापों को अपने में समाविष्ट करती जाती है। यह प्रक्रिया प्रत्येक के लिए भिन्न-भिन्न स्तर पर जाकर रुक जाती है। लाखों में से कोई एक विरली आत्मा ही इस आदर्श स्थिति के कुछ समीप जा पाती है। अब यह शुरुआत होती किस प्रकार है? यह एक बहुत ही विस्तृत विषय है और प्रत्येक के लिए विशिष्ट होता है। पर फिर भी इसमें कुछ सामान्य बातें हैं जिनके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं।
जब व्यक्ति को किसी प्रकार सच्चे रूप से यह समझ में आ जाए कि वर्तमान जीवन तो स्वार्थमय है जहाँ सारे दिन वह केवल मन, प्राण और शरीर की संतुष्टियों की पूर्ति में ही लगा रहता है, तब वह समझ जाता है कि केवल प्रभु को निवेदित जीवन ही जीने योग्य है। ऐसी समझ उसे पूर्वजन्म के संस्कारों के द्वारा, किसी सत्संग के द्वारा, किसी पुस्तक के अध्ययन के द्वारा, जीवन में घटी किसी अकस्मात् घटना के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से आ सकती है। हालाँकि अभी भी व्यक्ति अनेकानेक तरीके के भावों, विचारों, अपने कर्तव्यों, प्रतिबद्धताओं आदि से जकड़ा रहता है इसलिए आरंभ में अधिक कुछ नहीं कर पाता, परंतु फिर भी, जिस भी तरह हो, जब यह बात समझ में आ जाती है तो उसकी कुछ न कुछ छाप उसके जीवन पर अवश्य लग जाती है। इसलिए अन्य सभी कुछ के होते हुए भी व्यक्ति कहीं-न-कहीं यह प्रयास करना आरंभ करता है कि यह तत्त्व भी जीवन में प्रवेश करे। अब चूँकि इस चीज का अपना आकर्षण ही ऐसा है कि उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में उसे महसूस होता है कि यही चीज करने लायक है। पर इसके साथ ही साथ अधिकांशतः व्यक्ति को लगभग यह पूरा विश्वास हो जाता है कि वह तो भगवान् का हो चुका है। हालाँकि यह बात सत्ता के किसी एक भाग का सत्य अवश्य होता है परंतु फिर भी अभी भी व्यक्ति इस स्थिति से तो बहुत दूर होता है जहाँ वह वास्तव में ही भगवान् का हो चुका हो। पर यह बात भी व्यक्ति को तब समझ में आती है जब उसे जीवन में अनेक बार ठोकरें लगती हैं और उसकी सच्चाई कसौटी पर उतारी जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने साधना-पथ अपना लिया है और जो अपना सर्वस्व श्रीमाताजी की सेवा में अर्पित करने का संकल्प कर चुके हैं और जो वास्तव में भीतर से ऐसा करना चाहते भी हैं उन्हें भी कदम-कदम पर अपनी निम्न प्रकृति के धोखों से गुजरना होता है। क्योंकि यह बात तो बहुत देर से समझ में आती है कि हमारे बाहरी भागों को हमारे आंतरिक भाव से विशेष कोई सरोकार नहीं होता। इसलिए भीतर तो हमारे अंदर अपने आप को भगवान् को दे देने का भाव होता है परंतु बाहरी भागों के अपने निहित हेतु होते हैं इसलिए बाहरी अभिव्यक्ति के अंदर तो इन बाहरी भागों की ही प्रधानता रहती है। इतना अवश्य है कि यह भाव जीवन को कुछ रंग दे देता है। परंतु इस अवस्था में और पूर्ण समर्पण की अवस्था में एक बड़ा भारी अंतर होता है। हालाँकि सामान्य व्यक्ति को तो यह रंगत भी बड़ी प्रभावी प्रतीत होती है। ऐसा व्यक्ति अपने मित्र के लिए, देश के लिए अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं करता, अपने आदर्श के लिए प्राण भी दे सकता है। परंतु एक दृष्टिकोण से किसी आदर्श के लिए अपने प्राण दे देना अवश्य ही श्रेष्ठ तो है परंतु उसके लिए जीना और आवश्यक कष्ट सहन करना अधिक मुश्किल है। और सच्चा मूल्य तो ऐसे ही जीवन का है। सामान्यतया कुछ व्यक्ति दंभ भरते हुए या अपने प्रेम की प्रगाढ़ता दिखाते हुए कहते हैं कि वे श्रीमाताजी के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। पर वास्तव में तो श्रीमाताजी के लिए अपने सर्वस्व की आहुति देना कहीं अधिक महत् और कष्टकर है अन्यथा प्राण तो बिना कुछ किये भी अपने समय से चले जाते हैं। अवश्य ही श्रीमाताजी के लिए प्राण देने के भाव का अपना मूल्य है, परंतु उनके हेतु संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर दिया जाए और उनका सच्चा यंत्र बना दिया जाए, यह बेहतरं चीज है।
जब व्यक्ति के अंदर यह भाव हो कि वह भगवान् के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है तब तो सामान्यतः वह पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि अब वह पूरी तरह से भगवान् का हो चुका है। और इसके साथ ही साथ अपने विषय में व्यक्ति में बड़ी ही आत्म-तुष्टि और अपनी श्रेष्ठता का भान आए बिना नहीं रहता। और इस कारण व्यक्ति अपनी कमियों को देखने में असमर्थ हो जाता है जबकि दूसरों की कमियों को खूब देख लेता है। परंतु चूँकि अंदर कहीं न कहीं कुछ सच्चाई भी होती है इसलिए जब भगवान् की कृपा से वह अपनी अवस्था के विषय में कुछ अधिक सचेतन होता है तो वह उसके अनुसार यथासंभव अपने दृष्टिकोण आदि में परिवर्तन करता है। कुछ समय बाद वह पाता है कि पहले जिन धोखों के प्रति वह सचेतन हुआ था और जिन्हें उसने निकाल बाहर करने का प्रयास किया था उनका केवल रूप ही बदला है और वे कुछ अधिक सूक्ष्म बन गए हैं परंतु वे फिर भी उसके अंदर विद्यमान हैं। इस प्रकार व्यक्ति इन जाल-घातों की खोज करता रहता है, इनके प्रति सचेतन होकर इनका निराकरण करने का प्रयास करता रहता है और अपने पथ पर अग्रसर होता रहता है। परंतु यह निश्चित है कि प्रत्येक के साथ उसके अपने निम्न भागों की क्रीड़ा लगी रहती है जो उसे उसके गठन के अनुसार धोखे में रखती है। भगवान् का सत्य अनंत आयामी है अतः मानवीय चेतना का उसकी तरफ बढ़ना कठिनाईयों, अर्ध-सत्यों व प्रतीतियों से भरा होता है। धोखा शब्द यही इंगित करता है। इसलिए एक साधक यह निश्चित मान कर चले कि उसके साथ कहीं न कहीं धोखा अवश्य हो रहा है और इसलिए समझदारी इसी में है कि यह खोजे कि वह धोखा कहाँ खा रहा है और उससे बचने का प्रयास करे।
यहाँ गीता जिस भेंट की बात करती है उसे जब व्यक्ति व्यवहार में उतारता है तब वह पाता है कि इसके साथ ही साथ ऐसे भागों की क्रिया भी चलती रहेगी जो उसे जगह-जगह धोखा देते रहेंगे। परंतु अपनी केंद्रीय सच्चाई के आधार पर यदि व्यक्ति सभी लड़खड़ाहटों के बावजूद भी चलता रहे तब धीरे-धीरे वे धोखे कम होते जाते हैं। हालाँकि इन धोखों को हम इस रूप में ले सकते हैं कि ये हमें हमारी कमियों के बारे में सचेतन बनाते हैं। एक समय के बाद जब व्यक्ति अपने निम्न भागों पर कुछ-कुछ अंकुश लगा देता है तब वे भाग उठ खड़े होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं क्योंकि सचेतन रूप से तो व्यक्ति उन्हें अभिव्यक्ति का उतना अवसर नहीं देता। और जब कोई संकटकाल आता है, या किसी आकस्मिक घटना के कारण कोई आघात लगता है या अन्य किसी कारण से कोई मर्मांतक पीड़ा होती है तब इन भागों को सिर उठाने का मौका मिल जाता है। और श्रीमाताजी के अनुसार तभी सही समय होता है जब व्यक्ति इन्हें पकड़कर बाहर कर सकता है क्योंकि अन्य समय तो ये सभी भाग अँधेरे में छिपे रहते हैं और दिखाई नहीं देते। पर जब ये अपना सिर उठाएँ तब व्यक्ति को इनसे हताश या परेशान होने की बजाय इसे एक सुअवसर के रूप में देखना चाहिये क्योंकि तभी वह इनका सामना कर इनका सफाया कर सकता है। परंतु यह इतना आसान काम नहीं है और इसके लिए बड़े भारी विवेक, साहस और आत्मा की ताकत की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, रामायण में उल्लेख आता है कि जब भगवान् श्रीराम नागपाश में बंध गए तब विभीषण से उसका उपाय पूछने पर उसने कहा कि उसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसे समय में लक्ष्मण जी के अंदर एक दबा हुआ भाव फूट पड़ा और उन्होंने श्री रामजी से कहा कि जब कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी तभी उन्होंने उन्हें चेताया था कि कैकेयी की बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु तब तो उन्होंने उनके इस परामर्श को अनसुना कर दिया था, इसलिए आज वे सब ऐसे भीषण संकट में फंस गए हैं। हालाँकि गरुड़ के आने पर जब वे नागपाश से मुक्त हो गए तब लक्ष्मण जी को अपने भाव पर शर्मिंदा नागपारा से सकार तो जो भाव उनके अंदर लंबे समय से दवा था यह बाहर आ ही गया। इसी प्रकार हमारे अंदर भी ऐसी असंख्यों चीजें छिपी रहती हैं जो अपने समय की प्रतीक्षा करती हैं। इसीलिए साधना पथ पर ज्यों-ज्यों व्यक्ति आगे बढ़ता है त्यों-ही-त्यों अपने अंदर छिपी अनेकानेक चीजों की वह खोज करता है। और इसका एक परम लाभ यह है कि व्यक्ति अपने आप को अधिक सचेतन रूप से जानने लगता है तो कम से कम किसी निश्चित स्तर तक वह धोखा नहीं खाता। इसलिए गीता जिस भाव की बात कर रही है वह तो एक प्रकार से भाव की परिणति है। जिस तक सहज ही नहीं पहुँचा जा सकता। साधना पथ में हमें अपने इट की या गुरु की सहायता से अपने विभिन्न भागों के विषय में सचेतन होना होता है और जो भाग भगवान् की ओर खुले हैं उनके प्रकाश से दूसरे भागों को निर्मल करना होता है।
इस प्रकार यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भगवान् हमारे किसी एक भाग में प्रकाश फैला कर उसके द्वारा अन्य भागों को भी प्रकाशित और पवित्र करते हैं। भगवान् उस भाग को व्यक्ति की आत्मा का अधिकार जमाने के लिए एक माध्यम बना लेते हैं। आरंभ में यह प्रक्रिया बड़ी हो कष्टकर प्रतीत होती है, परंतु एक सीमा के बाद जब कुछ भाग प्रकाशित हो उठते हैं तब यह प्रक्रिया कुछ गति पकड़ लेती है। इसलिए ज्यों-ज्यों व्यक्ति आगे बढ़ता है उसकी गति भी त्वरित होती जाती है क्योंकि भगवान् का अधिकार क्षेत्र बढ़ता जाता है। और जब चैत्य चेतना जागृत होती है तब तो अपनी अंदर की किसी भी समस्या पर, किसी भी अवांछित चीज पर या किसी गुत्थी पर नजर भर डालनी होती है और उसका प्रकाश और प्रभाव इतना अधिक होता है कि वह चीज तुरंत ही समाप्त हो जाती है या फिर हल हो जाती है। वही समस्या जो हमें एक लंबे समय से प्रताड़ित कर रही थी और जिससे मुक्त होने के लिए हम प्रयास अवश्य कर रहे थे परंतु उन प्रयासों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उससे मुक्ति दिला सकें, वही क्षण भर में भी समास हो सकती है क्योंकि चैत्य सत्ता में बड़ी भारी शक्ति होती है और उसके समक्ष किसी त्रुटि आदि के बने रहने की कोई सामर्थ्य नहीं होती। परंतु फिर भी साधना पथ पर ये समस्याएँ अनगिनत हैं और व्यक्ति को इनका सामना करते रहने के लिए अनंत धैर्य की आवश्यकता होती है।
संक्षेप में, जो माँग हम से की गई है वह यही है कि हम अपने सम्पूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में बदल दें। हमारी सत्ता के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक क्रिया को शाश्वत के प्रति एक सतत् और समर्पित आत्मदान में परिणत करना होगा। हमारे सभी कर्मों को, छोटे-से-छोटे और अत्यन्त साधारण एवं तुच्छ कर्मों को तथा बड़े-से-बड़े और अत्यन्त असाधारण एवं श्रेष्ठ कर्मों को, सभी को एक समान, समर्पित कर्मों के रूप में करना होगा। हमारी व्यष्टिभूत प्रकृति को एक ऐसी बाह्य तथा आन्तर क्रिया की अखंड चेतना में निवास करना होगा जो ऐसे 'कुछ' के प्रति निवेदित हो जो हम से परे और अहं से महान् है। भले ही कोई भी भेंट-उपहार क्यों न हो और हमारे द्वारा किसी को भी भेंट की जा रही हो, परंतु भेंट की क्रिया में एक ऐसी चेतना अवश्य होनी चाहिये कि हम इसे सब सत्ताओं में विद्यमान एकमेव दिव्य परम सत्ता को ही भेंट कर रहे हैं। हमारे अत्यन्त साधारण और अत्यंत स्थूल रूप से भौतिक कार्यों को भी यही उदात्त रूप धारण करना चाहिये; जब हम भोजन करें, तो हमें सचेतन होना चाहिये कि हम अपना भोजन अपने अन्दर विराजमान उस दिव्य 'उपस्थिति' को दे रहे हैं; यह मन्दिर में एक पवित्र भेंटस्वरूप होना चाहिए और महज एक शारीरिक आवश्यकता का बोध या आत्म-तृप्ति का भाव हममें से चला जाना चाहिये।
सामान्यतया इस प्रकार की बातों को हम एक उद्देश्य के रूप में मान बैठते हैं कि हमारा भोजन उस दिव्य उपस्थिति को अर्पित होना चाहिये, आदि-आदि। परंतु ये सारी चीजें किसी आंतरिक चेतना की स्थिति के बाहरी परिणाम हैं। इस प्रकार का वर्णन पढ़ते ही अधिकांशतः लोग इसे व्यावहारिक जीवन में लागू करने की सोचते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, परंतु जिसे हम उद्देश्य मान बैठते हैं वह तो एक परिणाम है जो कि यदि हम साधना पथ पर चलते हैं तो स्वयमेव ही सिद्ध हो जाएगा। जब व्यक्ति उस चेतना में होगा तो स्वतः ही उसकी क्रिया-कलाप, भोजन आदि सभी प्रभु को ही समर्पित होंगे। इस दृष्टिकोण से हमें इसे लेना चाहिये अन्यथा इन निषेधाज्ञाओं को पढ़कर व्यक्ति के भाव उठता है कि अब वह समझ गया है कि उसे क्या करना चाहिये। परंतु केवल अध्ययन मात्र से हमारी अशिष्ट प्रकृति बदल नहीं जाती बल्कि उस ज्ञान की आड़ में तो सामान्यतया उसे अपनी क्रिया अधिक करने का मौका मिल जाता है। भारतीय संस्कृति में हमारी इस अशिष्ट प्रकृति का भली-भाँति ज्ञान था। इसीलिए संन्यासी के लिए ऐसे विधान थे जिनकी सहायता से वह किसी भी प्रकार की आसक्ति से अधिक से अधिक बच सके। संन्यास के बाद उसे अपने मूल निवासस्थान में रहने की अनुमति नहीं थी। इससे उसके सभी पारिवारिक बंधनों में उसकी आसक्ति टूट जाती थी। पिक्षा के अन्न पर जीने के विधान के कारण अहं पर भी बहुत कुछ अंकुश लगता था, साथ ही भोजन के प्रति तृष्णा को भी मौका न मिलने पर वह भी अंकुश में रहती थी। भौतिक सुख-साधन आदि पर भी अंकुश लग जाता था। हालाँकि इस प्रकार के अंकुश का प्रत्येक के लिए सुखद परिणाम नहीं होता।
परंतु इस प्रकार के अंकुश से भी भौतिक प्रकृति मान नहीं जाती। इसीलिए बाहरी अंकुश कुछ के लिए कुछ हद तक लाभदायक हो सकते हैं परंतु इनके द्वारा पूरी तरह से प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी के कारण श्रीअरविन्द अतिमानसिक चेतना के अवतरण और भौतिक प्रकृति तक के रूपांतरण की बात करते थे। केवल अतिमानसिक रूपांतरण के द्वारा ही वास्तव में हमारी प्रकृति की समस्याओं का अंत हो सकता है। अन्यथा बड़ी भारी सिद्धियाँ प्राप्त करने पर भी व्यक्ति की बाहरी प्रकृति में विशेष बदलाव नहीं आता, अपितु जो अधिक समय समाधिस्थ अवस्था में ही बिताना चाहते हैं उनकी बाहरी प्रकृति तो, श्रीमाताजी के अनुसार, बहुत अधिक निरंकुश और अशिष्ट हो जाती है और इसी कारण वे लोग बाहर की चेतना में आना ही नहीं चाहते और केवल अपनी समाधि अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं। परंतु जो भी हो, यदि व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी पूँजी है उसकी सहायता से मार्ग पर चल पड़े तो भले कितने भी उतार-चढ़ाव क्यों न आएँ, वह अधिकाधिक मार्ग पर आगे बढ़ता ही जाएगा।
किसी भी महान् प्रयास में, किसी भी उच्च अनुशासन में अथवा किसी कठिन या उदात्त पुरुषार्थ में - चाहे वह हमारे अपने लिए हो, दूसरों के लिए हो या फिर जाति के लिए हो - यह अब और अधिक सम्भव नहीं रह जाएगा कि हम जाति के, अपने-आप के या दूसरों के विचार तक ही आकर रुक जाएँ। जो काम हम कर रहे हैं उसे सचेतन रूप से कर्मों के यज्ञ के रूप में अर्पित करना होगा, पर इन्हें (अपने-आप को, दूसरों को या जाति को) नहीं, अपितु इनके द्वारा या सीधे ही एकमेव देवाधिदेव को अर्पित करना होगा, जो दिव्य अन्तर्वासी इन रूपाकृतियों के द्वारा छिप गया था उसे अब और अधिक छिपे नहीं रहना चाहिये, अपितु हमारी आत्मा, हमारे मन और हमारे इंद्रियबोध के समक्ष सदा उपस्थित रहना चाहिये। हमारे कर्मों की आंतरिक क्रियाओं और परिणामों को उस 'एकमेव' के हाथों में इस भावना से सौंप देना होगा कि वह 'उपस्थिति' ऐसी 'अनन्त' और 'परमोच्च' है कि केवल उसके द्वारा ही हमारे प्रयत्न तथा हमारी अभीप्सा सम्भव या चरितार्थ हो सकती हैं। क्योंकि उसी की सत्ता में सब कुछ घटित होता है; उसी के लिये प्रकृति द्वारा हमसे समस्त प्रयत्न और अभीप्सा लेकर सब को उसी की वेदी पर अर्पण किया जाता है। उन चीजों में भी जिनमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकृति स्वयं कर्ती होती है और हम उसकी क्रिया के केवल साक्षी, धारक और सहायक मात्र होते हैं, उनमें भी हमें कर्म और उसके दिव्य स्वामी का ऐसा ही अखंड स्मरण और स्थिर ज्ञान रहना चाहिये। हमारे अंदर के श्वास-प्रश्वास तक को, हमारे हृदय की धड़कन मात्र तक को भी वैश्विक यज्ञ के सजीव लय-ताल के रूप में सचेतन बनाया जा सकता है और बनाना ही होगा।
यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का विचार और इसका कारगर अभ्यास अवश्य ही अपने अंदर तीन परिणाम लिये रहता है जो हमारे आध्यात्मिक आदर्श के लिये केंद्रीय महत्त्व के हैं। सर्वप्रथम यह प्रत्यक्ष है कि यदि ऐसा अभ्यास बिना भक्ति के भी प्रारंभ किया जाए तो भी वह सम्भवनीय उच्चतम भक्ति की ओर सीधे और अनिवार्य रूप से ले जाता है; क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से गहरा होकर एक पूर्णतम कल्पनीय आराधना एवं अत्यन्त गंभीर ईश्वर-प्रेम में परिणत हो जाएगा। इससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा है सब वस्तुओं में भगवान् का अधिकाधिक अनुभव, हमारे समस्त चिंतन, इच्छाशक्ति एवं कर्म में तथा जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान् के साथ उत्तरोत्तर गहरा होता समागम और हमारी सम्पूर्ण सत्ता का भगवान् के प्रति अधिकाधिक भावपूर्ण निवेदन। वस्तुतः, कर्मयोग के ये निहितार्थ सर्वांगीण और पूर्ण भक्ति के भी सारतत्त्व हैं। जो जिज्ञासु इन्हें जीवन्त अभ्यास में डाल देता है वह अपने-आप में निरंतर ही आत्मोत्सर्ग के सच्चे भाव की एक स्थायी, सक्रिय और प्रभावशाली प्रतिमूर्ति निर्मित करता रहता है, और यह अनिवार्य ही है कि इसमें से फिर उस सर्वोच्च देव की अत्यन्त मग्न करनेवाली पूजा का जन्म हो जिसे यह सेवा अर्पित की जाती है। उस दिव्य उपस्थिति के लिए, जिसके प्रति समर्पित कार्यकर्ता सदा उत्तरोत्तर प्रगाढ़ सामीप्य अनुभव करता है, उसमें अनन्य प्रेम बढ़ता जाता है। और इसके साथ ही सभी सत्ताओं, जीवित रूपों एवं प्राणियों के लिये, जो भगवान् के वास-स्थान हैं, एक सार्वभौम प्रेम भी पैदा होता है। वह इस अनन्य प्रेम के अन्दर निहित रहता है - यह कोई विभाजन से उत्पत्र क्षणिक, व्याकुल एवं ग्रसित करने वाला भावावेग नहीं होता, अपितु उह सुस्थिर निष्काम प्रेम होता है जो एकत्व का गंभीरतर स्पन्दन होता है। सभी चे जिज्ञासु अपनी सेवा और आराधना के एकमात्र पात्र से मिलन साधित करने लगता है। कर्मों का मार्ग यज्ञ के इस पथ से चल कर भक्ति के मार्ग से जा मिलता है; यह स्वयं ही एक ऐसी परिपूर्ण, तन्मयकारी और सर्वांगीण भक्ति हो सकता है, जिसकी कि हृदय माँग कर सकता हो या जिसकी मन का प्रवर भाव कल्पना कर सकता हो।
अब यहाँ यह एक बड़ी ही विचित्र बात है कि यह अभ्यास बिना भक्ति के किस प्रकार आरंभ किया जा सकता है। सामान्यतया भक्ति हृदय से उद्भूत होती है। परंतु यदि हृदय के द्वारा वह भाव प्रकट रूप से अभिव्यक्त न हो जिसे हम भक्ति कहते हैं अपितु अंतरात्मा में एक अभीप्सा हो जो कि हमें परमात्मा की ओर प्रेरित करती है तब भी यह प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। भले ही हमारी परंपरागत शब्दावली में किसी हठयोगी या किसी तपस्वी की क्रिया को भक्ति की संज्ञा नहीं दी जाती, तब भी यह निश्चित है कि अंतरात्मा में कहीं न कहीं किसी उच्चतर चीज के लिए अभीप्सा अवश्य होती है। इस प्रकार जब व्यक्ति हृदय के बिना अंतरात्मा के किसी प्रकार के दबाव के कारण किसी ज्ञान आदि से भी आरंभ करता है तब कम से कम उसे कुछ थोड़ा-बहुत आधार प्राप्त होता है जिसके सहारे वह मार्ग पर चलना आरंभ करता है। हालाँकि बिना हृदय के भाव के उस गति में तीव्रता नहीं आती, परंतु यदि कोई थोड़ा-बहुत प्रयास भी आरंभ हो गया हो तो वह भी धीरे-धीरे प्रबल होता जाएगा और सत्ता के अन्य भागों को प्रभावित कर अपने में सम्मिलित करता जाएगा और अंततः अवश्य ही इस गति की पराकाष्ठा भक्ति में होगी। यही गीता की साधना की विशिष्टता है कि यह किसी भी भाग से आरंभ कर धीरे-धीरे सभी भागों को अपने में समाविष्ट कर लेती है और संभवतः एक ऐसी भक्ति में इसकी परिणति होगी जो कदाचित् भक्तियोग से आरंभ करने वाले साधक के लिए भी दुर्लभ हो। गीता की साधना सामान्य भक्तियोग या ज्ञानयोग या कर्मयोग से सर्वथा परे की चीज है और इसका अभ्यास अन्य सभी पारंपरिक योगों की सीमाओं से परे ले जाता है। इसी की श्रीअरविन्द यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि जिसे प्रचलित तौर पर भक्ति कहते हैं - जिसमें व्यक्ति अतिशय रूप से भगवान् के प्रति आकृष्ट हो, या फिर जिसमें दास्य, सख्य आदि भाव हों और जिसमें मिलन-विरह आदि उतार-चढ़ाव आ रहे हों, जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक पूजा-अर्चना आदि में रत रहता हो - यदि व्यक्ति भक्ति के ऐसे किन्हीं भी बाहरी लक्षणों के बिना भी कहीं न कहीं आत्मा की क्षीण-सी भी अभीप्सा के बल पर आरंभ करता है तो भले कितना भी लंबा समय क्यों न लगे, तो भी आवश्यक रूप से इस गति की परिणति भक्ति में ही होगी। यह भक्ति की एक ऐसी पराकाष्ठा होगी जिसमें व्यक्ति हर चीज में, हर घटना में, हर क्षण अपने प्रेमास्पद के ही दर्शन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति में किसी भी प्रकार की एकांगिता नहीं रहती, किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं रहती अपितु सर्वसमावेशी भाव आ जाता है जिसके प्रभाव से ज्ञान अपनी सभी सीमाएँ लाँघ जाता है क्योंकि तब सारा ब्रह्माण्ड ही भगवान् का मंदिर बन जाता है। इसीलिए यह एक ऐसी परिपूर्ण, तन्मयकारी और सर्वांगीण भक्ति होती है, जिसकी कि हृदय माँग कर सकता हो या जिसकी मन का प्रबल भाव कल्पना कर सकता हो, क्योंकि हृदय की माँग होती है अपने प्रेमास्पद से सन्निकटता और इस अनुभूति में तो भगवान् सतत् ही उसके साथ होते हैं। और जब व्यक्ति को सतत् परमात्मा के ही दर्शन होने लगते हैं तब उनके निमित्त कर्म करना सहज हो जाता है।
परन्तु इस प्रकार के भाव तक पहुँच पाना आसान नहीं है क्योंकि थोड़ा-बहुत आरम्भ करके व्यक्ति कहीं न कहीं रुक जाता है। जिस प्रकार के भाव की चर्चा गीता कर रही है वह बहुत ही विशिष्ट है। ऐसे किन्हीं भी वर्णनों में हमें सदा ही यह याद रखना चाहिये कि ये सभी वर्णन निरूपण की किसी एक पद्धति विशेष का अनुसरण करते हैं क्योंकि किसी भी मानसिक निरूपण की यह बाध्यता है कि वह किसी एक धारा के अनुसार विकसित होता है जबकि जिस वास्तविक पथ से व्यक्ति आरोहण करता है वह प्रत्येक के लिए विशिष्ट होता है और बहुआयामी होने के कारण किसी भी प्रकार के मानसिक निरूपण से सर्वथा परे होता है। अतः यहाँ जो वर्णन है वह समझने की दृष्टि से उत्तम है परंतु वास्तविक यात्रा उससे कहीं अधिक विचित्र और श्रेष्ठतर होती है जिसका कोई भी वर्णन संभव नहीं है।
प्रश्न : यहाँ पर श्रीअरविन्द जो वर्णन करते हैं वह तो उनका अपना अनुभव रहा होगा?
उत्तर : श्रीअरविन्द केवल इतना कहते हैं कि यह एक संभव मार्ग जिससे व्यक्ति अग्रसर हो सकता है। वे कहीं भी ऐसा नहीं कहते कि यही एकमात्र मार्ग है। परमात्मा की क्रियाओं को कोई भी व्यक्ति समझ हो। कैसे सकता है क्योंकि इस संसार को देखने का सब का अपना अलग-अलग दृष्टिकोण है। पशु-पक्षियों का अपना दृष्टिकोण है, मनुष्यों का अपना दृष्टिकोण है और मनुष्यों में भी प्रत्येक की चेतना के स्तर के अनुसार उन्हें संसार भिन्न-भिन्न दिखाई देता है। इतना कह सकते हैं कि उच्चतर चेतना के स्तर पर दृष्टिकोण श्रेष्ठतर होता है। और कोई भी वर्णन अधिक से अधिक केवल कुछ दिशानिर्देश तो दे सकते हैं परंतु आवश्यक नहीं कि व्यक्ति की यात्रा उसके अनुसार चले। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का पथ भी कभी एक जैसा नहीं होता। एक ही गुरु के दो अनुयायियों तक का विकासक्रम एक जैसा नहीं होता। इसलिए जब व्यक्ति साधना-पच पर अग्रसर होता है तब आवश्यक नहीं कि उसके अनुभव ऐसे किन्हीं भी वर्णनों से मेल खाते हों जो उसने पूर्व में पढ़ या सुन रखे थे। इतना अवश्य है कि यदि व्यक्ति का भगवान् के प्रति लगाव है तो वह जिस किसी भी पथ से अवश्य ही उनकी ओर बढ़ता ही जाएगा।
परंतु इससे यह अर्थ भी नहीं निकाल लेना चाहिये कि ये सब वर्णन निरर्थक हैं। अवश्य ही इनका अपना बड़ा भारी महत्त्व है। परंतु इस प्रकार की चीजों को एक संतुलित तरीके से लेने की आवश्यकता है परंतु चूंकि सामान्यतया बुद्धि में इतनी परिपक्वता नहीं होती इसलिए व्यक्ति ऐसे वर्णनों को संतुलित रूप tilde F नहीं ले पाता। हमें सदा ही यह ध्यान रखना चाहिये कि किन्हीं भी मानसिक सूत्रों में निरूपित करते ही कोई भी सत्य अपने सर्वांगीण स्वरूप का बहुत कुछ खो बैठता है। परंतु फिर भी इन सत्यों का निरूपण किया जाना लाभदायक हो सकता है।
इसके बाद, इस योग का अभ्यास एकमात्र केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान के सतत् आन्तरिक स्मरण की माँग करता है, और इसके साथ ही इस स्मरण को प्रगाढ़ बनाने के लिए कर्म में इस ज्ञान की निरन्तर सक्रिय मूर्त रूपों में अभिव्यक्ति सम्मिलित हो जाती है। सब में एक ही आत्मा है, एकमेव भगवान ही सब कुछ हैं; सब भगवान् में हैं, सब भगवान् हैं और विश्व में भगवान् के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है - यह विचार या यह श्रद्धा तब तक कार्यकर्ता का संपूर्ण आधार या पृष्ठभूमि रहती है जब तक कि यह उसकी चेतना का संपूर्ण तत्त्व ही नहीं बन जाती। इस प्रकार के स्मरण को, अपने-आप को क्रियाशील बनाने वाले इस प्रकार के ध्यान को अंत में उसके – जिसका हम इतने शक्तिशाली रूप से स्मरण करते हैं अथवा इतने अनवरत रूप से ध्यान करते हैं, - प्रगाढ़ और निर्बाध दर्शन तथा जीवंत और सर्वसमावेशी चेतना में बदल जाना चाहिये और निश्चय ही यह बदल भी जाता है। क्योंकि यह प्रत्येक क्षण समस्त सत्ता, संकल्प और कर्म के उद्गम से संबद्धता रखने के लिए बाध्य करेगा और इसके साथ ही एकाएक सभी विभिन्न रूपों तथा प्रतीतियों का उस 'तत्' में, जो इनका कारण और धर्ता है, ग्रहण और अतिक्रम हो जाता है। यह मार्ग विश्वव्यापी आत्मा की कृतियों को सर्वत्र ही स्पष्ट एवं सजीव रूप में, भौतिक रूप में देखने के समान ही प्रत्यक्ष रूप में, बिना देखे अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच सकता। अपनी चरमावस्था में यह अतिमानस, परात्पर की उपस्थिति में सतत् निवास, चिंतन, संकल्पन और कर्म-निष्पादन की स्थिति तक उठ जाता है। जो कुछ हम देखते और सुनते हैं, जो कुछ भी हम स्पर्श करते और अनुभव करते हैं, जिस सब के विषय में हम सचेतन हैं, उस सब को हमें उसी वस्तु के रूप में जानना और अनुभव करना होगा जिसकी हम पूजा और सेवा करते हैं; सभी को भगवान् की प्रतिमा में परिणत करना होगा, सभी को उसे उसके देवता के निवासधाम के रूप में देखना होगा तथा शाश्वत सर्वव्यापकता से आवरित करना होगा। बहुत पहले भी नहीं तो अपनी समाप्ति के समय यह कर्ममार्ग, भागवत् उपस्थिति और संकल्प एवं बल के साथ अन्तर्मिलन होने पर, एक ज्ञानमार्ग में बदल जाता है जो ऐसे किसी भी मार्ग से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण होता है जिसे कोरी मानवी मति रच सकती है या बुद्धि की खोज उपलब्ध कर सकती है।
और यह सब वर्णन भी गीता की जो परिणति है, 'सर्वधर्मान्परित्यज्य', उसका एक सीमित रूप है क्योंकि जिस 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' की स्थिति तक गीता उठा ले जाती है वह तो किसी भी ऊँची से ऊँची मानवीय कल्पना से परे की स्थिति है। उसका तो कोई ओर-छोर ही नहीं है। परंतु अधिकांशतः किसी स्थिति विशेष पर पहुँचने पर व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसने सभी धर्मों को, अपने सभी ढाँचों या संरचनाओं को पूर्णतया भगवान् को अर्पित कर दिया है और पूर्णता प्राप्त कर ली है। हमारे मानवीय मन को यह आभास नहीं होता कि जिसे वह पूर्णता मानता है वह तो कोई प्राणिक या मानसिक आडंबर मात्र हो सकता है जो चकाचौंध करने वाले रूपों में अपने आप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। सच्ची पूर्णता केवल यही हो सकती है कि हमारे द्वारा परम प्रभु का संकल्प निर्बाध रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। हमारा बाहरी आवरण उस संकल्प की अभिव्यक्ति में यदि कोई बाधा डालता है तो इसका अर्थ है कि पूर्णत्व की स्थिति अभी स्थापित नहीं हुई है। इसलिए 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' की स्थिति में पूर्णता दिव्य विधान के अनुसार होती है न कि हमारे मानकों के अनुसार और जब यह स्थिति आती है तब हो सकता है कि उसकी बाहरी अभिव्यक्ति किन्हीं वर्णनों के अनुरूप प्रतीत होती हो और यह भी संभव है कि वह किन्हीं भी वर्णनों से सर्वथा परे हो। क्योंकि जब तक वह स्थिति नहीं आती तब तक तो व्यक्ति को लगता है कि वह किन्हीं आधारों की सहायता से, किसी मार्ग विशेष के अनुसार अग्रसर हो रहा है, परंतु जब व्यक्ति के द्वारा दिव्य संकल्प बिना किन्हीं विकृतियों के अभिव्यक्त होने लगता है तब उसका अपना ही विधान होता है और वह हमारे किन्हीं भी विधानों और वर्णनों की पकड़ में नहीं आता। श्रीअरविन्द पर भी यदि हम अपने मानवीय मानदण्डों को प्रयुक्त करने का प्रयास करें तो वे भी कदाचित् ही उनमें खरे उतरेंगे क्योंकि हमारे ऊँचे से ऊँचे मानदंड भी बहुत ही दकियानूसी होते हैं। इसलिए पूर्णता आदि स्थितियों के संबंध में व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं जबकि सच्ची चीज उन सभी विचारों और धारणाओं से परे रहती है। सामान्यतया इसी प्रकार की प्रचलित धारणाओं के कारण योग में निर्विकल्प समाधि आदि अवस्थाओं को बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता रहा है। ऐसी ही योग की कुछ पुस्तकें पढ़ने पर स्वयं श्रीमाताजी को यह शंका उठी कि उन्हें तो कभी उस प्रकार की स्थितियों के अनुभव नहीं प्राप्त हुए जिनका उन पुस्तकों में वर्णन मिलता है। श्रीअरविन्द से मिलने पर जब यह शंका उन्होंने उनके समक्ष प्रकट की तो श्रीअरविन्द ने कहा कि स्वयं उन्हें भी कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं हुआ है। अतः जब हम पारंपरिक योग आदि की पुस्तकें पढ़ते हैं तब उनमें अनेक प्रकार की समाधि अवस्थाओं के वर्णन पाते हैं और हमारे अंदर ऐसी धारणाएँ बैठ जाती हैं मानो वे अवस्थाएँ अवश्य ही योग की बहुत ऊँची अवस्थाएँ होंगी। परंतु श्रीअरविन्द ने इस विषय पर अपने पत्रों में यह स्पष्ट किया है कि प्रायः ऐसी समाधि अवस्थाएँ सच्ची अवस्थाएँ न होकर अचेतनता में गिरना ही होता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति किसी तरह सूक्ष्म प्राणिक या मानसिक जगत् में प्रवेश करता है परंतु वहाँ सचेतन बने रहने की क्षमता न होने के कारण जड़वत् हो जाता है। इसलिए वास्तव में इसका व्यक्ति पर कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब क्रीड़ास्थल में श्रीमाताजी ध्यान कर रही थीं और अतिमानसिक अवतरण हुआ तब एक दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ उस समय विद्यमान भौतिक वस्तुओं को भी अतिमानसिक चेतना का स्पर्श प्राप्त हुआ था। परंतु यह तो कोई भी समझ सकता है कि आखिर उन वस्तुओं में उस चेतना को ग्रहण करने की कितनी क्षमता हो सकती थी? इसी प्रकार जिन समाधि आदि अवस्थाओं का वर्णन पढ़ने-सुनने में आता है वे अधिकतर तो ऐसी अवस्थाओं के ही वर्णन हैं जिनमें व्यक्ति सचेतन नहीं रह पाता और उसे वह समाधि अवस्था की संज्ञा दे देता है। जब श्रीअरविन्द ने अतिमानसिक योग की घोषणा की तब लोगों ने यह कहते हुए इसका उपहास किया कि योगियों को तो बहुत पहले से ही सच्चिदानंद के स्तर तक के अनुभव प्राप्त होते रहे हैं और वे तो अभी भी उससे बहुत निचले स्तर, अतिमानस, की ही बात कर रहे हैं। तब श्रीअरविन्द ने स्पष्ट किया कि अवश्य ही सच्चिदानंद का अनुभव सुदीर्घ काल से प्राप्त होता रहा है परंतु अभी तक ऐसा आधार तैयार नहीं था जहाँ कि उसे उसके सच्चे वैभव में ग्रहण किया जा सके। उदाहरण के लिए किसी विषय में पारंगत शिक्षक यदि शिशुओं की कक्षा को पढ़ाने के लिए जाएँ तो भला अपने ज्ञान का कितना अंश वे उन शिशुओं को दे पाएँगे। वहीं योग्य छात्र उनके ज्ञान को अधिक ग्रहण कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। यही श्रीअरविन्द का कहना है कि केवल अतिमानस के आने पर ही अध्यात्म को सच्चा आधार प्राप्त होगा जहाँ मुक्त रूप से वह अपनी क्रिया कर सके। उससे पहले हमारी मानवीय चेतना में तो उसकी क्रिया बाधित हो जाती है। इसी के कारण उन्होंने अतिमानसिक रूपांतरण को अपरिहार्य और अवश्यंभावी बताया।
इसलिए वास्तव में करने योग्य एक ही सच्ची चीज है और वह है अपने आप को पूर्ण सच्चाई के साथ अपने गुरु को, श्रीमाताजी को समर्पित कर देना और इतने पूर्ण रूप से समर्पित कर देना कि कोई अभीप्सा आदि करना भी निरर्थक परिश्रम प्रतीत हो क्योंकि तब अन्य कोई अभीप्सा रहती ही नहीं। जब हम भगवान् से भक्ति आदि की माँग करते हैं तब भी अधिकांशतः तो हम अपने आप के अहं के ऊपर ही केंद्रित रहते हैं और उसी की पुष्टि का प्रयास कर रहे होते हैं। इसीलिए श्रीमाताजी कहती हैं कि भगवान् को देखने की, उन्हें प्राप्त करने की अतिशय उत्कंठा भी उनके और हमारे बीच एक आवरण का काम कर सकती है। अतः सच्ची चीज है अपने आप को पूर्णरूपेण श्रीमाताजी के हाथों में, भगवान् के हाथों में सौंप देना और फिर वे जैसे चाहें वैसे निर्वाध रूप से हमारे अंदर और हमारे द्वारा अपना संकल्प अभिव्यक्त करें। जब तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार की स्पृहा रहती है, भले ही वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, तब तक वह हमारी अज्ञानमय अवस्था को हो दर्शाती है क्योंकि परमात्मा के अंदर किसी प्रकार की स्पृहा नहीं हो सकती और यदि हम उनसे सच्चे रूप से जुड़े हैं, उनके प्रति समर्पित हैं और उन्हीं का संकल्प हमारे द्वारा अभिव्यक्त होता है तो हमारे अंदर भी स्पृहा नहीं रह सकती। इसलिए स्पृहा होना हमारी अपरिपक्व अवस्था का सूचक है।
अन्त में, यज्ञ-रूपी इस योग का अभ्यास हमें अपने मन, संकल्प और कर्म में से अहंभाव के समस्त आन्तरिक अवलंबनों को त्यागने के लिए और अपनी प्रकृति में से इसके बीज, इसकी उपस्थिति एवं इसके प्रभाव को निकाल फेंकने के लिए बाध्य करता है। सब कुछ भगवान् के लिये ही करना होगा; सभी कुछ को भगवान् की ओर ही लक्षित करना होगा। एक पृथक् सत्ता के रूप में स्वयं के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए; चाहे पड़ोसी, मित्र और परिजन हों, अथवा देश या मानवजाति या अन्य प्राणी हों, दूसरों के लिये भी महज इसलिए कुछ न करना चाहिए कि वे हमारे निजी जीवन, विचार और भावुकता से सम्बद्ध हैं, अथवा इसलिए कि हमारा अहं स्पृहा के वशीभूत हो उनकी भलाई में अधिक रुचि रखता है। कर्म तथा विचार के इस तरीके से सभी कार्य और समस्त जीवन भगवान् की अपनी विराट् वैश्व सत्ता के निःसीम मन्दिर में उसकी दैनिक सक्रिय आराधना और सेवा ही बन जाते हैं। जीवन व्यक्ति में शाश्वत का अधिकाधिक एक ऐसा यज्ञ बनता जाता है जो अनवरत एक सनातन परात्परता के प्रति स्वयमेव अर्पित होता रहता है। यह सनातन विश्वगत आत्मा के क्षेत्र की विशाल यज्ञीय भूमि में अर्पित किया जाता है; और शाश्वत शक्ति या सर्वव्यापिनी माता ही स्वयं इसे अर्पित करती है। अतएव, यह मार्ग कर्मों द्वारा और कर्मगत भाव तथा ज्ञान द्वारा मिलन एवं समागम प्राप्त करने का मार्ग है, और यह वैसा ही पूर्ण और सर्वांगीण है जैसा हमारी ईश्वराभिमुख इच्छाशक्ति आशा कर सकती है, अथवा जैसा हमारी आत्म-शक्ति कार्यान्वित कर सकती है।
इसके अंदर एक सर्वांगीण और परम कर्मयोग के मार्ग की समस्त शक्ति विद्यमान है, परंतु दिव्य आत्मा और स्वामी के प्रति अपने यज्ञ और आत्मोत्सर्ग के विधान के कारण, यह मार्ग एक ओर तो प्रेममार्ग की संपूर्ण शक्ति से युक्त होता है और दूसरी ओर ज्ञानमार्ग की संपूर्ण शक्ति से सम्पन्न होता है। इसके अन्त में ये तीनों दिव्य शक्तियाँ एक-दूसरे से घुल-मिलकर और एकीभूत, परिपूरित एवं पूर्ण होकर एक साथ काम करती हैं।
जिन अनुभवों का श्रीअरविन्द यहाँ वर्णन कर रहे हैं वे सभी संभव हैं और अवश्य ही लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं। परंतु स्वयं अपने बारे में श्रीअरविन्द बताते हैं कि आरंभ से ही उन्होंने अपने गुरु के निर्देशानुसार अपने अंतःस्थित परम पथप्रदर्शक को पूर्ण रूप से समर्पित करने का मार्ग अपनाया जिसे कि श्रीरामकृष्ण परमहंस बिल्ली के शावक के भाव का रूपक देते थे क्योंकि बिल्ली का शावक बिना किसी चिंता के अपनी माँ के भरोसे रहता है और माँ उसे अपने मुँह में लेकर सुरक्षित रूप से जहाँ कहीं ले जाना होता है वहाँ ले जाती है। साथ ही, जो लोग समर्पण का मार्ग अपनाते हैं उन सब का भी अपना-अपना विशिष्ट विकासक्रम होता है। किसी पद्धति-विशेष का अनुसरण करने वालों में भी सब का अपना-अपना भिन्न विकास होता है। उदाहरणार्थ, श्रीअरविन्द आश्रम में समान ही गुरु की छत्रछाया में रहते हुए भी सभी के अपने-अपने इतने भिन्न प्रकार के अनुभव थे जो कि हमें श्रीअरविन्द के योग-विषयक पत्रोत्तरों में पढ़ने को मिलते ही हैं। इसलिए भले कोई भी मार्ग हो, पर व्यक्ति को सदा ही यह भान होना चाहिये कि हमारे अंदर परमात्मा जो विकासक्रम अपनाते हैं उसे किन्हीं भी मानसिक सूत्रों में न तो बाँधा जा सकता है और न ही उनकी सहायता से समझा ही जा सकता है।
प्रश्न : तब फिर जिन चीजों के विषय में हम यह सब वर्णन पढ़ रहे हैं उसके लिए हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए?
उत्तर : इन सबसे हमें यह तो अवश्य ही समझ लेना चाहिये कि पथ पर ये सब संभावनाएँ हैं या ऐसे संभव पड़ाव हैं जो किसी साधक को मिल सकते हैं। परंतु यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति इन्हीं के द्वारा होकर गति करेगा। सभी का अपना विशिष्ट मार्ग होता है, हालाँकि ये जितनी भी संभावनाएँ हैं उनका भी कुछ-कुछ अनुभव व्यक्ति को मार्ग में हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं कि वह अनुभव उसी क्रम से हो जिस क्रम से उसका वर्णन होता है। परंतु एक बार अपने आप को अपने गुरु के हाथों में सौंपने के बाद किसी प्रकार की व्यक्तिगत चेष्टा, जैसे कि अमुक प्रकार की साधना पद्धति या अभ्यास अपनाने की चेष्टा यह दिखलाती है कि व्यक्ति ने वास्तव में अपने आप को अपने गुरु को या इष्ट को सौंपा नहीं है बल्कि वह तो केवल यह सौदेबाजी ही कर रहा है कि किस में उसे कितना लाभ मिल सकता है। अवश्य ही, यदि भीतर से किसी प्रकार के चयन करने की अनुमति या आज्ञा हो तब तो व्यक्ति अवस्थानुसार यथोचित चयन कर सकता है अन्यथा नहीं। परंतु श्रीअरविन्द जिस प्रकार के समर्पण के मार्ग का यहाँ वर्णन कर रहे हैं यदि व्यक्ति वास्तव में उसका अनुसरण करे तो उसे यह भ्रम भी नहीं हो सकता कि व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बल पर वह स्वयं कुछ कर सकता है क्योंकि कदम-कदम पर उसे यह महसूस होगा कि क्रिया तो वही करनी है जो श्रीमाताजी कहेंगी, या प्रेरणा देंगी। सामान्यतः व्यक्ति जब साधना का कोई मार्ग अपनाता है तब वह विचार करता है कि अमुक प्रकार का अभ्यास करने से अमुक परिणाम प्राप्त होगा, या फिर किसी ध्यान-विशेष का अभ्यास करने से कोई अन्य प्रकार के लाभ या परिणाम प्राप्त होंगे। इस सब में व्यक्ति परिणाम को ध्यान में रखता है और उसी के अनुसार चेष्टाएँ करता है। परन्तु जब हम समर्पण का मार्ग अपनाते हैं तब उसमें ऐसे क्रिया-कलाप नहीं रहते। इसमें तो व्यक्ति सदा ही किसी दूसरी शक्ति की क्रिया के लिए खुला होता है जो कि अपने ही निराले विधान के अनुसार उसे अग्रसर करती है जो उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित हो सकता है। इसीलिए इसमें व्यक्ति को निज पुरुषार्थ का भ्रम भी नहीं होता। इस प्रकार के सच्चे समर्पण के मनोभाव में व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार के अभ्यास आदि करने की आंतरिक चेष्टाएँ नहीं रहतीं क्योंकि सब कुछ तो दिव्य संकल्प के हाथों में होता है और यही तो सच्ची स्वतंत्रता है जिसमें कि व्यक्ति को निज पुरुषार्थ का और उसके परिणामों का बोझ नहीं ढोना पड़ता चाहे बाहर से देखने में उसका जीवन कितना भी कठोर साधनामय जीवन क्यों न प्रतीत होता हो। वह तो निश्चेष्ट रूप से जगज्जननी की क्रिया के प्रति खुला होता है और शुरू में केवल उन्हें अपने द्वारा अधिकाधिक निर्बाध रूप से कार्य करने देने का प्रयास करता है।
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ।
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।। २८॥
२८. इस प्रकार तू शुभ-अशुभ फल-रूप कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा; और संन्यास के द्वारा भगवान् के साथ आत्मा में युक्त होकर तू मुक्त हो जाएगा
और मुझे प्राप्त हो जाएगा। तब कामना और अहंकार के बनाए हुए भेद मिट जाते हैं। क्योंकि अपने कर्म के शुभ फल की व्याकुलता नहीं होती, और दुःखद परिणाम से अलगाव नहीं होता अपितु समस्त कर्म और फल उन परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है जिनके कि जगत् के सारे कर्म और फल सदा से हैं, इसलिए (कर्म करनेवाले भक्त के लिए) कर्म का कोई बन्धन नहीं होता। क्योंकि एक पूर्ण आत्म-दान के द्वारा सारी अहंकारमय कामना हृदय से मिट जाती है और जीव के पृथक् जीवन के आन्तरिक संन्यास के द्वारा भगवान् और व्यष्टिगत आत्मा (जीव) के बीच पूर्ण एकत्व सिद्ध हो जाता है। संपूर्ण संकल्प, संपूर्ण कर्म, सम्पूर्ण फल भगवान् के हो जाते हैं, और ये विशुद्ध और प्रबुद्ध प्रकृति के द्वारा दिव्य रूप से क्रिया करते हैं और अब ये सीमित व्यक्तिगत अहं से संबद्ध नहीं रह जाते। इस प्रकार समर्पित प्रकृति अनन्त की एक मुक्त वाहिका बन जाती है; जीव अपनी आध्यात्मिक सत्ता में, अज्ञान और बन्धन से ऊपर निकलकर सनातन पुरुष के साथ अपने एकत्व में लौट आता है।
यहाँ जब भगवान् कहते हैं कि 'तू शुभ-अशुभ फल-रूप कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा', तब हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह शुभ और अशुभ केवल हमारी अहमात्मक चेतना के लिए होता है। भगवान् की क्रिया तो स्वाभाविक रूप से सदा ही शुभ है। यदि हम परमात्मा की चेतना से जुड़े हों तो हमें कुछ भी अशुभ नहीं लगता। परंतु चूँकि हम एक पृथक् अहं की दृष्टि से देखते हैं जबकि जगत्-व्यापार हमारे अहं के दृष्टिकोण से नहीं चलता, इसलिए जब कोई चीज अहं को अनुकूल लगती है तब हम उसे शुभ की संज्ञा दे देते हैं और जब वह प्रतिकूल लगती है तब उसे अशुभ कह देते हैं। हमारे सभी सुखों-दुःखों का भी यही कारण है। हालाँकि इस श्लोक से यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिये कि जिसे हम अशुभ कहते हैं सब के लिए उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु वह उस व्यक्तिविशेष की चेतना से मिट जाएगा जो भगवान् से युक्त है। जब व्यक्ति भगवान् के प्रति समर्पित होगा और उनके लिए कर्म करेगा तब वह शुभ-अशुभ से मुक्त हो जाएगा। और समर्पित होने का लक्षण है व्यक्ति को अपने इष्ट की क्रिया में आनन्द आने लगता है। यदि यह समर्पण सहर्ष न हो पर ईश्वर की इच्छा के प्रति शांत अधीनता का भाव ही हो तब व्यक्ति शांत भाव से उनकी इच्छा को शिरोधार्य तो करता है परंतु उसे उसमें आनन्द नहीं आता। आनन्द तो तब आता है जब उसे उनसे इतना प्रेम हो कि उनकी सभी क्रियाएँ अच्छी लगने लगे। जब एक माँ अपने बच्चे की शरारतों को देखती है तो भले ही बाहर से वह जो भी भाव दर्शाती हो परंतु भीतर से उसे अपने बच्चे की सभी शरारतों से सुख की अनुभूति होती है। जब मानवीय आसक्ति ही सारे दृष्टिकोण को बदल सकती है तब यदि सच्चा प्रेम हो तब तो अपने प्रेमास्पद की क्रिया में आनन्द आना स्वाभाविक ही है। यह एक मूलभूत मनोवैज्ञानिक भाव है जिसमें हमारी चेतना शुभ-अशुभ से सर्वथा परे हो जाती है और उसे चीजें उस दृष्टिकोण से गोचर ही नहीं होतीं। परंतु यह तो एक सर्वथा भिन्न स्थिति है जिसे प्राप्त करना सहज नहीं है। इसलिए सामान्यतः जो अर्थ लगाया जाता है कि व्यक्ति को अच्छे-बुरे, शुभ-अशुभ के बीच कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता, वह सही नहीं है क्योंकि यह भेद न देख पाना किसी दिव्यता की नहीं अपितु जड़ता की निशानी है। अतः जब तक व्यक्ति के अंदर अहमात्मक चेतना है तब तक उसे चयन करना ही होगा, विवेक रखना ही होगा। परमात्मा की चेतना से युक्त होने पर भी चयन तो करना ही होता है, परंतु वह चयन शुभ-अशुभ, अच्छे-बुरे या हमारे अन्य किन्हीं भी मानवीय मानदंडों के आधार पर नहीं होता। वह तो दिव्य जननी के विधान के अनुसार होता है। पर फिर भी चयन तो करना ही होता है। उदाहरण के लिए सड़कें अपने आप में कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होतीं परंतु हमें अपने गंतव्य के अनुसार उनमें से चयन करना होता है। वही सड़क किसी समय हमारे गंतव्य के अनुसार अनुकूल हो सकती है और अन्य किसी समय उसके प्रतिकूल हो सकती है। इसलिए यह कहना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और बेतुकी बात होगी कि चूँकि हमारे अंदर समता आ गई है इसलिए हम सभी सड़कों के प्रति समान भाव रखकर किसी पर भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे भौतिक रूप से इस बात का बेतुकापन हमें महसूस होता है वैसे ही थोड़े से विकास और परिष्करण के द्वारा हमें मनोवैज्ञानिक विषयों में सामान्यतया हम जिस प्रकार की बिल्कुल बेतुकी बातें करते हैं उनका कुछ-कुछ भान होने लगता है। अतः न तो परमात्मा ही सनकों के अनुसार चलते हैं और न ही वे लोग अपनी सनकों के अनुसार चलते हैं जो परमात्मा से युक्त हैं।
व्यक्ति की प्रकृति में भले जो भी कोई गुत्थियाँ, गाँठें आदि हों, पर यदि एक बार उसके यह समझ में आ जाता है कि वह अपनी सच्ची सत्ता के बिना नहीं जी सकता और वह भगवान् से ऐक्य साधने के मार्ग पर चल पड़े तो सहज ही उसे ज्ञान आ जाता है। एक बार यह भाव आने पर फिर मूलभूत रूप से तो इन गुत्थियों आदि की समस्या समाप्त हो जाती है क्योंकि फिर तो यह केवल इस पर निर्भर करता है कि उस मार्ग पर व्यक्ति कितनी तीव्रता से चलता है। उस मार्ग की ओर उन्मुख होना, उस पर चल पड़ना ही सबसे मूलभूत बात है। एक बार जब यह यात्रा आरंभ हो जाए तब तो फिर केवल उसमें लगने वाले समय की ही बात है। वहीं, यदि बाहरी प्रकृति दिखने में बड़ी सुसंस्कृत भी हो, गुणसंपन्न भी हो, परंतु जिसमें भगवान् से ऐक्य का यह संकल्प न आया हो तो सब वृथा है और वास्तव में उसका अधिक कोई मूल्य नहीं होता। अतः मूल बात यही है कि जब तक व्यक्ति अपनी सच्ची सत्ता से नहीं जुड़ जाता, उसका अपना जो सच्चा स्वरूप है वही नहीं बन जाता, तब तक उसकी दुविधाओं का अंत नहीं हो सकता और होना चाहिये भी नहीं अन्यथा तो जिस उद्देश्य से आत्मा इस अभिव्यक्ति में आई थी वही निष्फल हो जाएगा। वास्तव में तो हमारे दुःख-कष्ट, दुविधाएँ आदि सभी भगवान् की असीम अनुकंपा के ही बाहरी चिह्न हैं क्योंकि यदि ये दुःख कष्ट न होते तो हम सदा अपनी स्थिति से चिपटे रहते और उसे छोड़ने की और उसका अतिक्रमण कर ऊर्ध्व आरोहण करने की कभी सोच ही नहीं सकते थे और केवल अपनी वर्तमान क्षुद्र भौतिक, प्राणिक और मानसिक अवस्था में ही संतुष्ट रहते और कभी दिव्य जीवन की ओर प्रयाण नहीं करते। इसी कारण हम देखते हैं कि भौतिक कष्ट से भी अधिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक कष्ट पीड़ादायक होता है। एक गहरे विश्लेषण के द्वारा हम देखते हैं कि इस पीड़ा का होना हमारी आत्मा को जीवित रखने के लिए आवश्यक ही है अन्यथा तो बाहरी लबादा कभी उसके प्रस्फुटन को मौका ही नहीं देता। यही कारण है कि जिन्हें सारी भौतिक सुख-सुविधाएँ उपलब्ध हैं उन्हें भी दुःख-कष्ट और यंत्रणा, मनोवैज्ञानिक और आंतरिक क्षुधाएँ आदि घेरे रहती हैं। क्योंकि ये क्षुधाएँ किन्हीं भी भौतिक सुख-सुविधाओं से शांत नहीं होतीं। ये तो केवल अपनी आत्मा के संपर्क में आने से, हम जो सच्चे रूप में हैं वही बन जाने से ही मिट सकती हैं।
प्रश्न : भौतिक दुःख-कष्ट तो हम समझते हैं, पर मानसिक और प्राणिक पीड़ाएँ क्या होती हैं?
उत्तर : प्राणिक पीड़ाओं के पीछे प्राणिक जगत् की सत्ताएँ होती है जो हमें अपने उपयोग में लेकर अपनी संतुष्टि खोजती हैं। बिल्कुल निम्म कोटि की प्राणिक सत्ताओं को तो केवल काम-वासना आदि से पैदा होने वाले स्पंदनों में ही रस आता है। उससे कुछ ऊपर की सत्ताओं को अपने इंद्रिय भोगों की पूर्ति में रस आता है। प्रायः हम देखते हैं कि किस प्रकार लड़के-लड़कियों के बीच प्राणिक आदान-प्रदान एक आम चीज बन गई है। पाश्चात्य संस्कृति में तो यह चीज हमें निरंकुश रूप से भड़को हुई दिखाई देती है। भारत में भी इसका अब पूरा प्रभाव है। इन सभी प्राणिक संबंधों के पीछे प्राणिक सत्ताएँ रस लेती हैं। उन्हें उस स्पंदन में भी उतना ही रस आता है जिसे हम मानव प्रेम कहते हैं जितना कि आपसी लड़ाई झगड़े, कलह, यंत्रणा, आत्म-दया आदि के स्पंदनों में। अब चूंकि वर्तमान संस्कृति मुख्य रूप से प्राणिक इच्छाओं-कामनाओं के इर्द-गिर्द ही घूमती है इसलिए सब जगह इनकी तुष्टि की एक अंधाधुंध दौड़ दिखाई देती है। परंतु इन प्राणिक इच्छाओं का स्वभाव ही यह है कि ये अतृप्य हैं और इस कारण इनका पीछा करते-करते मनुष्य का जीवन असंतोष और यंत्रणा से भर जाता है।
परंतु इससे भी अधिक पीड़ा मनोवैज्ञानिक होती है। जब व्यक्ति को जीवन निःसार लगने लगता है और उसके वर्तमान जीवन के तौर-तरीकों में कोई आशा नजर नहीं आती तब यह अत्यंत पीड़ादायक स्थिति होती है। यह पीड़ा तो इतनी तीव्र हो सकती है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाए। इसी से अत्यंत पीड़ित होने के कारण इससे कुछ राहत की खोज में हम बढ़ती संख्या में पाश्चात्य लोगों को बहुत तीव्र गति से भारतीय आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते देखते हैं। आज कदाचित् हो ऐसा कोई देश होगा जहाँ कि भारतीय गुरुओं का जाना और वहाँ से जिज्ञासुओं का आध्यात्मिक परामर्श के लिए भारत आना न होता हो। कुछ लोगों को जिन्हें मुक्ति का यह द्वार नहीं प्राप्त होता वे अपनी इस पीड़ा से बचने के लिए प्रायः मादक पदार्थों के सेवन की ओर भी बढ़ जाते हैं और अंततः अपना सर्वनाश कर बैठते हैं। वास्तव में तो जब तक हम परमात्मा को नहीं पा लेते तब तक हमारे दुःखों का कभी अंत नहीं हो सकता क्योंकि परमात्म सत्ता ही हमारा सच्चा स्वरूप है इसलिए जब तक हम अपने निजस्वरूप में न आकर किसी अन्य के भेष को ही धारण किये रहते हैं तब तक हमें सुख कैसे मिल सकता है।
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ।। २९।।
२९. मैं समस्त भूतों में समान हूँ, मुझे कोई भी प्रिय नहीं है और कोई द्वेष का पात्र नहीं है; तथापि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें हूँ।
दिव्य शाश्वत सब भूतों में वासी हैं: सब में वे सम हैं और सभी प्राणियों के समान रूप से मित्र, पिता, माता, रचयिता, प्रेमी और भर्ता हैं। वे किसी के भी शत्रु नहीं और किसी के पक्षपातपूर्ण प्रेमी नहीं हैं; किसी को भी उन्होंने बहिष्कृत नहीं किया है, किसी को सदा के लिए अपराधी घोषित नहीं कर दिया है, किसी पर उन्होंने कोई निरंकुश स्वेच्छाचारी सनक के द्वारा अनुग्रह नहीं किया हैः सब समान ही रूप से अज्ञान में अपने-अपने चक्कर काटकर अन्त में उन्हीं के पास आते हैं। परंतु केवल यह पूर्ण भक्ति ही है जो ईश्वर का मनुष्य में और मनुष्य का ईश्वर में जो निवास है उसे एक सचेतन क्रिया और एक तन्मयकारी और पूर्ण ऐक्य में परिणत कर सकती है। परमोच्च का प्रेम और एक पूर्ण आत्मसमर्पण ही इस दिव्य एकत्व का सीधा और द्रुत मार्ग है।
...जितना अधिक तुम अपने-आप को भगवान् को देते हो उतना ही अधिक वे तुम्हारे साथ होते हैं, पूर्ण रूप से, सतत् रूप से, प्रतिक्षण, तुम्हारे सभी विचारों में, सभी आवश्यकताओं में, और ऐसी कोई अभीप्सा नहीं होती जो तत्क्षण उत्तर न प्राप्त करती हो; और तुममें एक पूर्ण, सतत् घनिष्ठता का, एक पूर्ण निकटता का भाव रहता है। यह ऐसा है मानो तुम (उन्हें) अपने साथ लिये होते हो ... मानो भगवान् हर समय तुम्हारे साथ हों; तुम चलते हो तो वे तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम सोते हो और वे तुम्हारे साथ सोते हैं, तुम खाते हो तो वे तुम्हारे साथ खाते हैं, तुम सोचते हो और वे तुम्हारे साथ सोचते हैं, तुम प्रेम करते हो और वे वही प्रेम हैं जो तुम प्राप्त करते हो। परंतु इसके लिये व्यक्ति को अपने-आप को पूरे तौर पर, संपूर्ण रूप से, अनन्य रूप से देना होगा, अपने-आप के लिए कुछ भी बचाकर न रखना होगा, अपने-आप के लिये और अपने पास कुछ भी न रखना होगा, और साथ ही किसी चीज को बिखेरना नहीं हैः तुम्हारी सत्ता में छोटी-से-छोटी चीज भी जो भगवान् को नहीं दी गयी है वह बर्बादी है; यह तुम्हारे आनन्द की बर्बादी है, एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे सुख को उतना कम कर देती है, और जो कुछ तुम भगवान्क नहीं देते वह वैसा ही है मानो भगवान् अपने-आप को तुम्हें दे सकें इस संभावना के मार्ग में तुम उसे खड़ा कर देते हो। तुम उन्हें अपने सत्रिको संभात तुम्हारे साथ अनुभव नहीं करते क्योंकि तुम उनके नहीं हो, क्योंकि देर सैंकड़ों अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों के हो; तुम्हारे विचार में, तुम्हारी क्रिया है। तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे आवेशों में... लाखों-लाखों ऐसी चीजें हैं जो तुम उन्हें नहीं देते, और इसीलिये तुम उन्हें सदा अपने साथ अनुभव नहीं करते क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारे और उनके बीच इतने सारे पर्दे और दीवारें है परंतु यदि तुम उन्हें सब कुछ दे दो, यदि तुम कुछ भी बचाकर न रखो, तो तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी अनुभव करते हो उसमें सदा, हर क्षण, वे सतत् और पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ होंगे।
यह हमारे समर्पण की एक अद्भुत कसौटी है। यदि हम भगवान् की सतत् उपस्थिति अनुभव नहीं करते तो यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि हम परमात्मा के प्रति नहीं अपितु अपने अहं के प्रति समर्पित हैं। यह एक सुनिश्चित आध्यात्मिक अनुभव है कि यदि व्यक्ति अपने आप को भगवान् को पूरी तरह दे देता है तो वह उनकी सतत् उपस्थिति अनुभव करता है। एक प्रसंग आता है जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए। जब वे श्रीराधा रानी के पास उन्हें ज्ञान देने के उद्देश्य से गए और समझाने लगे कि उन्हें भगवान् के लिए विरह नहीं करना चाहिये तो श्रीराधा रानी ने कहा कि भगवान् तो सतत् ही उनके साथ हैं और उन्हें छोड़कर तो वे कभी कहीं गए ही नहीं और न कभी कहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही यह प्रसंग भी आता है कि जब उद्धव जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो प्रमाणस्वरूप राधारानी ने उन्हें भगवान् के दर्शन करा दिये। यह देखकर तो उद्धव जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कहने का अर्थ है कि जिसे इस सतत् उपस्थिति का अनुभव होता है वही जानता है कि किस प्रकार हर छोटी से छोटी चीज में भी व्यक्ति को भगवान् की सतत् उपस्थिति अनुभव होती है। श्रीमाताजी ने स्वयं के जीवन का अनुभव बताते हुए कहा कि जब तक श्रीअरविन्द भौतिक शरीर में उपस्थित थे तब तक कभी भी उन्हें गंभीर से गंभीर काम करने पर भी कभी भार नहीं अनुभव हुआ और लगभग तीस सालों तक वे सदा ही श्रीअरविन्द की चेतना के अवलंब के द्वारा बिल्कुल निश्चिंत रूप से अपनी क्रिया करती थीं। श्रीअरविन्द की चेतना सतत् ही उनके साथ थी। क्षण भर के लिए भी कभी उन्होंने उनकी उपस्थिति का अभाव नहीं महसूस किया। परंतु उनका संबंध तो प्रेम से भी अधिक प्रगाढ़ था क्योंकि यह तो दो शरीरों में एक ही तत्त्व के विद्यमान होने की अनुभूति है जिसकी प्रगाढ़ता की कल्पना नहीं की जा सकती। जब व्यक्ति का किसी भी भाव से भगवान् से प्रेम हो जाए तब भी बहुत ही आनन्द का अनुभव होता है परंतु यदि एक ही तत्त्व दो शरीरों में अभिव्यक्त होता हो तब तो उस परम आनन्द की अनुभूति का तो वर्णन ही नहीं हो सकता।
इसीलिए श्रीमाँ कहती हैं कि, "तुम्हारी सत्ता में छोटी-से-छोटी चीज भी जो भगवान् को नहीं दी गयी है वह बर्बादी है; यह तुम्हारे आनन्द की बर्बादी है, एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे सुख को उतना कम कर देती है, और जो कुछ तुम भगवान् को नहीं देते वह वैसा ही है मानो भगवान् अपने-आप को तुम्हें दे सकें इस संभावना के मार्ग में तुम उसे खड़ा कर देते हो।" परंतु चूंकि हमारे अंदर बहुत से भगवद्विरोधी भाग हैं जो अपने आप को भगवान् को समर्पित करने से हमें रोकते हैं, इसलिए यदि इन सब भागों के कोलाहल को अनसुना करके हम भगवान् की ओर चल सकें, अपने आप को भगवान् को समर्पित कर सकें तो यह हमारी सच्चाई की परीक्षा और हमारी सच्चाई का प्रमाण होगा। यदि ये सभी विरोधी भाग न हों तो हमारी सच्चाई की कोई कसौटी ही नहीं रहेगी।
प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा को भी वशीभूत कर लेती है। इसीलिए श्रीअरविन्द एक स्थान पर कहते हैं कि परमात्मा सभी कुछ के मालिक हैं परंतु प्रेम के सेवक हैं। स्वयं भगवान् भी एक स्थान पर कहते हैं कि वे व्यक्ति को अन्य सभी वांछित चीजें तो दे देते हैं - जैसे कि ज्ञान, मान-सम्मान, साधन, शक्ति-सामर्थ्य, साधना, सिद्धि – परंतु अपनी भक्ति सहज ही नहीं देते। क्योंकि उससे तो वे स्वयं ही भक्त के वश में हो जाते हैं। वर्तमान में तो हमने अपनी सारी शक्तियाँ अपने मन, प्राण और शरीर के सुख साधन में, अहं के सुख साधन में, परिवार आदि में लगा रखी हैं। इसलिए भगवान् को देने के लिए तो हमारे पास लेशमात्र भी कुछ बचा नहीं रहता। इसीलिए भारतीय संस्कृति में संयम और निग्रह आदि अनुशासनात्मक पद्धतियाँ इतनी प्रचलित थीं ताकि यदि कुछ ऊर्जा संचित हो सके तो व्यक्ति भगवान् की ओर गति कर पाए। अन्यथा तो व्यक्ति अपने 'मैं' और 'मेरे' के भाव से इतना ग्रस्त होता है कि अपने से अलग कोई चीज उसे सुझती ही नहीं। जब व्यक्ति किसी तरह भगवान् की ओर मुड़ता भी है तब भी प्रायः बाह्य प्रकृति तो लगभग वैसी ही असंस्कृत प्रकार की रहती है। परंतु आत्माभिमान में व्यक्ति को यह पान ही नहीं होता कि उसकी प्रकृति इतनी असंस्कृत है। इसीलिए ऐसी प्रकृति को सुसंस्कृत बनाने में लंबा समय लगता है।
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।। ३० ।।
३०. यदि बहुत दुराचारी मनुष्य भी अनन्य और पूर्ण प्रेम के साथ मेरी ओर मुड़ता है तो उसे साधु ही मानना चाहिये क्योंकि उसमें प्रयत्न का सुदृद्ध संकल्प और प्रयास समुचित और पूर्ण हैं।
क्षिप्रं भवति धर्मात्माशश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।। ३१।।
३१. वह मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शान्ति को प्रास करता है। हे कौन्तेय! यह निश्चित जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।
हम सब के अन्दर समान रूप से जो भागवत् उपस्थिति है वह अन्य कोई प्राथमिक माँग नहीं करती यदि एक बार श्रद्धा और हृदय की सच्चाई के साथ तथा मूलभूत पूर्णता के साथ सर्वांगीण आत्मसमर्पण कर दिया जाए। यह द्वार सभी की पहुँच के भीतर है, सभी इस मंदिर के अन्दर प्रवेश कर सकते हैं: सर्वप्रेमी के इस प्रासाद में हमारे सारे सांसारिक भेद लुप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, पूर्ण आत्मसमर्पण का संकल्प आत्मा के सभी द्वारों को पूरा खोल देता है और इसके प्रत्युत्तर में मनुष्य" के अन्दर भगवान् का पूर्ण अवतरण और आत्मदान ले आता है, और यह एकाएक ही निम्न प्रकृति के आध्यात्मिक प्रकृति में त्वरित रूपान्तर के द्वारा हमारे अन्दर के सभी कुछ को
"यदि कोई भगवान् को चाहे तो भगवान् स्वयं उसके हृदय के शुद्धिकरण का भार ले लेंगे, साधना को आगे बढ़ाएँगे तथा आवश्यक अनुभव प्रदान करेंगे; यदि व्यक्ति में भगवान् पर भरोसा और विश्वास तथा समर्पण का संकल्प हो तो इस तरीके से घटित हो सकता है और होता ही है। क्योंकि भगवान् का इस प्रकार ग्रहण करना व्यक्ति के एकमात्र अपने निजी प्रयास पर निर्भर न होकर अपने-आप को भगवान् के हाथों में सौंप देने पर निहित है और इसके लिए अपरिहार्य है व्यक्ति का भगवान् पर भरोसा और विश्वास और उत्तरोत्तर आत्मदान। यही वास्तव में साधना का वह सिद्धांत है जिसका स्वयं मैंने पालन किया था और यही योग की केंद्रीय पद्धति है जिसकी मैंने परिकल्पना की है। मैं समझता हूँ कि यह लेकर भागवत् सत्ता के विधान के अनुरूप पुनर्गठित कर देता है और उसके सदृश बना देता है। आत्मसमर्पण का संकल्प अपनी शक्ति से ईश्वर और मनुष्य के बीच के पर्दे को हटा देता है; प्रत्येक भूल को मिटा देता और प्रत्येक विघ्न को नष्ट कर डालता है। जो लोग अपनी मानवी शक्ति के भरोसे ज्ञान-साधन या पुण्यकर्म अथवा कठोर आत्म-संयम द्वारा अभीप्सा करते हैं वे बड़े कष्ट से शाश्वत की ओर आगे बढ़ पाते हैं;
__________________________
वही चीज है जिसे श्रीरामकृष्ण ने बिल्ली-शावक की पद्धति के रूपक के द्वारा बतलायी थी। परन्तु सभी एकाएक इसका अनुसरण नहीं कर सकते; इस तक आने में उन्हें समय लगता है - यह सबसे अधिक तब विकसित होती है जब मन और प्राण शांत हो जाते हैं...
आंतरिक समर्पण का सारमर्म है भगवान् पर भरोसा और दृढ़ विश्वास। व्यक्ति यह मनोभाव अपनाता है : "मैं भगवान् को चाहता हूँ, और किसी चीज को नहीं। मैं पूर्णतः अपने को उन्हें दे देना चाहता हूँ और चूँकि मेरी अन्तरात्मा ऐसा चाहती है, इसलिए इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता कि मैं उनका साक्षात्कार पाऊँ और उन्हें उपलब्ध करूँ। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, बस, मेरे अन्दर होनेवाली उनकी क्रिया मुझे उन तक ले जाए, उनकी यह क्रिया चाहे गुप्त हो या प्रकट, प्रच्छन्न हो या मूर्त। मैं आग्रह नहीं करता कि ऐसा मेरे अपने समय और तरीके के अनुसार हो; भगवान् सब कुछ अपने समय और अपनी पद्धति से करें; मैं उनका विश्वास करूँगा, उनकी इच्छा को स्वीकार करूँगा, दृढ़ भाव से उनकी ज्योति, उपस्थिति और आनन्द के लिये अभीप्सा करूँगा, सभी कठिनाइयों और विलंबों के भीतर से गुजरूँगा, उन्हीं पर निर्भर रहूँगा और कभी उनका परित्याग नहीं करूँगा। मेरा मन शांत हो जाए और उन पर भरोसा करे और वे इसे अपनी ज्योति की ओर खोल दें: मेरा प्राण स्थिर हो जाए और एकमात्र उन्हीं की ओर मुड़ जाए और वे इसे अपनी शांति और हर्ष की ओर खोल दें। सब कुछ उनके लिये हो और स्वयं मैं भी उनके लिये होऊँ। जो कुछ हो, मैं इस अभीप्सा और आत्मदान के भाव को बनाये रखूँगा और इस पूर्ण भरोसे के साथ आगे बढ़ता रहूँगा कि यह संपन्न हो जाएगा।"
यही मनोभाव है जिसमें व्यक्ति को बढ़ना होगा; क्योंकि निश्चय ही इसे एकाएक ही पूर्ण नहीं बनाया जा सकता - मानसिक और प्राणिक क्रियाएँ आड़े आती हैं - परन्तु कोई यदि इसके लिये संकल्प बनाये रखे तो यह सत्ता में विकसित हो जाएगा। इसके बाद जो काम है वह है उस मार्गदर्शन का अनुसरण करना जब वह स्वयं को प्रकट करता है, और अपने मन और प्राण की क्रियाओं को उसमें बाधा न डालने देना।
परंतु जीव जब अपने अहंकार तथा कर्मों को भगवान् को समर्पित कर देता है तब भगवान् स्वयं हमारे पास आते हैं और हमारा भार वहन कर लेते हैं। अज्ञानी को वे दिव्य ज्ञान का आलोक, दुर्बल को दिव्य-संकल्प का बल, पापात्मा को दिव्य-पवित्रता की मुक्ति, दुःखी को अनन्त आत्मसुख और आनंद ला देते हैं। उनकी दुर्बलता तथा उनके मानवी बल की लड़खड़ाहट से (कृपा में) कोई अंतर हीं पड़ता। "यह मेरी प्रतिज्ञा है", भगवान् की वाणी अर्जुन को कह उठती है, "जो मुझसे प्रेम करता है उसका नाश नहीं होता।"
व्यक्ति सच्चा प्रेम करना सीखता हो तब है जब वह परमात्मा की ओर अभिमुख होता है। इससे पहले तो उसे केवल प्रेम का भ्रम होता है जब वह कहता है कि वह अपनी पत्नी से, या माता-पिता से, या अपने मित्र से या अन्य किसी से प्रेम करता है। किसी भी मनुष्य के लिए प्रेम करना असंभव है क्योंकि वह प्रेम के योग्य ही तब बनता है जब वह परमात्मा की ओर मुड़ता है। तभी उसके हृदय में कोई सच्ची चीज आ सकती है जिसके प्रभाव से फिर वह सबसे प्रेम कर सकता है। जिसे हम प्रेम कहते हैं वह तो वास्तव में जिन संबंधों में हम आसक्त हैं उनके साथ संसर्ग से हमें मिलने वाली संतुष्टि ही है जिसमें हमें वास्तव में किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही सरोकार होता है। इसी को हम प्रेम कहते हैं। इसलिए जब तक हम इन्हीं संसर्गों में आसक्त रहते हैं तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते।
प्रश्न : सामान्यतः हम अपने अंदर की अनेकानेक समस्याओं की चर्चा करते हैं जो हमें परमात्मा की ओर मुड़ने से रोकती हैं जैसे कि हमारा अहं, प्राणिक प्रकृति आदि। तो क्या ये सारी समस्याएँ व्यक्तिगत होती हैं या फिर ये हमारे क्रमविकास के द्वारा हमें मिली होती हैं, या फिर अन्य कुछ?
उत्तर : इसमें प्रश्न यह नहीं है कि ये समस्याएँ व्यक्तिगत हैं या सार्वजनिक, क्योंकि वास्तव में जिसे सतही रूप से हम व्यक्ति समझते हैं वह तो एक दृष्टिकोण से केवल एक मुखौटा या एक प्रतीति मात्र ही है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि वास्तव में तो परम प्रभु स्वयं ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमें तो अहं के कारण व्यक्तिगत पुरुषार्थ का आभास होता है। इसलिए वास्तव में तो हमें कुछ भी करने या न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु यह एक ऐसी बात है जिसका कि तामसिक प्रवृत्ति को उचित ठहराने के लिए भयंकर रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है। इसी कारण हमारे वैदिक ऋषि सदा सतर्क रहते थे कि किसी अनधिकारी को ऐसा कोई ज्ञान न दिया जाए जो उसका भयंकर दुरुपयोग कर स्वयं का नुकसान कर बैठे और दूसरों का भी नुकसान कर बैठे। वे सदा ही देश-काल-पात्र को अत्यंत महत्त्व देते थे। वही ज्ञान जो किसी एक व्यक्ति के लिए परम कल्याणकारी हो सकता है वही किसी दूसरे के संपूर्ण मानसिक गठन को विचलित कर सकता है और उसे विध्वंस की ओर ले जा सकता है। इतिहास में भी हमें ऐसे अनेकानेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ किसी सत्य को एकांगी रूप से ग्रहण करने के कारण बहुत से दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा है। जब तक हम अपनी मानसिक सीमाओं से बँधे हैं तब तक पूर्ण सत्य तक नहीं पहुँच सकते। इसी कारण मानसिक चेतना में जब हम सत्य के विषय में कोई कथन करते हैं तब उसका विपरीत कथन भी अपने स्थान पर उतना ही उचित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि सभी कुछ परमात्मा की ही इच्छा से होता है, तो इसका विपरीत कथन भी अपने समय और स्थान पर उतना ही उचित होता है कि परमात्मा की इच्छा से कुछ भी नहीं होता और व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने चयन के लिए स्वतंत्र है। अब यह व्यक्ति के विकास की अवस्था पर निर्भर करेगा कि उसके लिए कौनसा कथन उपयोगी होगा। सामान्यतया हमारा गठन तामसिक प्रकार का होता है इसलिए यह कहना कि व्यक्ति को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ ईश्वर की ही इच्छा से होता है, एक विपरीत दिशा में गति होगी। तामसिक प्रकृति के लिए तो यही सही है कि वह अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करे ताकि अपने तमस् से कुछ बाहर आ सके। अतः सभी कुछ व्यक्ति के विकास की अवस्था पर निर्भर करता है।
__________________
* आप जो नीचे के सभी जगतों को व्यापे हुए हैं
और फिर भी ऊर्ध्वस्थित हैं
उन सभी के स्वामी जो कर्म करते हैं, शासन करते हैं और ज्ञाता हैं
परंतु, प्रेम के सेवक!
प्रश्न : यहाँ पादटिप्पणी में कहा गया है कि, "यही मनोभाव है जिसमें व्यक्ति को बढ़ना होगा", तो वास्तव में मनोभाव का अर्थ क्या है?
उत्तर : हम कह सकते हैं कि मनोभाव का अर्थ है मन का आंतरिक भाव। यह भाव हमारे मस्तिष्क के बाहरी विचारों आदि से भिन्न होता है और संभव है कि यह भाव बहुत गहराई से आता हो, परंतु सामान्य जीवन में ऐसे भावों को अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराने का, अपनी वाणी सुनाने का अवसर ही नहीं मिल पाता क्योंकि मन के अंदर अनेकानेक तरीके के विचारों, कोलाहलों की आँधी-सी छाई रहती है जिसके कारण ये गहरे भाव उसके पीछे छिपे रह जाते हैं। परंतु जब व्यक्ति साधना पथ पर कुछ कदम भी चलता है तब ये भाव धीरे-धीरे उजागर होने लगते हैं। पले ही ये भाव आरंभ में अप्रकट ही रहते हैं, पर धीरे-धीरे ये प्रकट होने लगते हैं। जब हम श्रीमाताजी व श्रीअरविन्द की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, अथवा हमारे अन्य सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ऐसे मनोभावों को सहज ही प्रकट होने में सहायता मिलती है। हमारे अपने जीवन में हम देखते हैं कि जब हम श्रीअरविन्द के साहित्य का अध्ययन और मनन करते हैं तब हमारे अंदर भी प्रसुप्त मनोभाव जागृत हो उठते हैं और हमें महसूस होता है मानो वह हमारी आत्मा की ही वाणी हो जिसे श्रीअरविन्द ने प्रभावी रूप से शब्दों के द्वारा रूप प्रदान कर दिया हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में हमें कुछ आंतरिक स्पर्श प्राप्त होते हैं, कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, कुछ अंतर्बोध प्राप्त होते हैं, परंतु इनका हमें कहीं वर्णन नहीं मिलता। पर जब श्रीअरविन्द अथवा श्रीमाताजी की किसी पुस्तक के माध्यम से, या फिर अन्य किसी सग्रंथ के माध्यम से हमें वे ही अनुभव वहाँ वर्णन किये हुए मिलते हैं तो यह बड़ा ही रोमांचकारी और प्रकाशक होता है। स्वयं श्रीअरविन्द को जब अनेकों अनुभव हुए पर कहीं भी किसी साहित्य में उन्हें उनका उल्लेख नहीं मिला तब उन्हें किसी ने राय दी कि कदाचित् वेदों में उन्हें उनका वर्णन मिले। और जब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया तब पाया कि वे सारे अनुभव वेदों में अंकित थे। अपने अनुभवों के कारण ही उन्हें वेदों की कुंजी भी प्राप्त हुई और तभी उन्होंने वेदों के रहस्य को प्रकट किया। इसी प्रकार हमारे पुराणों में भी अनेकानेक तरीके के अनुभवों आदि का वर्णन है। परंतु उन्हें वास्तव में समझ पाने के लिए हमें स्वयं भी वे गहरे अनुभव होने आवश्यक हैं। पर इतना अवश्य है कि इस प्रकार के अध्ययन से अंदर के गर्भित या सुप्त पड़े भावों आदि को जागृत होने का, प्रकट होने का अधिक सुअवसर मिलता है। अतः जब हमारे मनोभाव हमें किसी सिद्ध पुरुष या अन्य किसी के द्वारा अभिव्यक्त किये मिलते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि हमारे हृदय की वाणी को हमारे गुरु के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा शब्द प्रदान किये जा रहे हैं। इसी प्रकार तो आत्म-अन्वेषण होता है। हमारे अंदर इतनी-इतनी तरीके की चीजें होती हैं जैसे कि हमारे विचार, भावनाएँ, कल्पनाएँ, अभीप्साएँ, पूर्वाग्रह, महत्त्वाकांक्षाएँ, लालसाएँ आदि, और ये सभी आत्मपरक होने के कारण आपस में इतनी घुली मिली होती हैं कि इनके अंदर सही-सही भेद कर पाना किसी के लिए भी सामान्यतः सरल नहीं होता। इसलिए इनमें वास्तव में किसका कितना मूल्य होना चाहिये यह तो हमें गुरु की वाणी से ही पता लग सकता है।
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ।। ३२ ।।
३२. हे पार्थ ! जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, वे अधम जाति के, पापयोनि से उत्पन्न, स्त्री, वैश्य, और शूद्र होने पर भी परम गति को प्राप्त होते हैं।
पहले का प्रयास और तैयारी, जैसे ब्राह्मण की शुचिता और पवित्रता, कर्म और ज्ञान में श्रेष्ठ राजर्षि का प्रबुद्ध बल इत्यादि, का अपना महत्त्व है क्योंकि वे अपूर्ण मानवजीव के लिए इस विशाल दर्शन और आत्मसमर्पण तक पहुँचना सरल बना देते हैं; परन्तु इस प्रकार की तैयारी के बिना भी वे सब जो मनुष्य के इन दिव्य-प्रेमी भगवान् की शरण लेते हैं, वह चाहे वैश्य हो जो किसी समय धनोपार्जन तथा उत्पादन-श्रम की संकीर्णता में ही चिंताकुल था, या शूद्र हो जो सहस्रों कठोर प्रतिबन्धों में आबद्ध था, या स्त्री हो जिसके आत्मविस्तार के चारों ओर खींचे गए समाज के एक संकुचित घेरे के कारण जिसकी उन्नति का मार्ग बराबर रुद्ध और प्रतिहत रहा है, ये ही नहीं अपितु वे पापयोनि भी जिनके ऊपर पूर्व-कर्म ने खराब-से-खराब जन्म लाद दिया है, जो जातिबहिष्कृत हैं, पैरिया या चाण्डाल हैं, ये सब के सब भी एकाएक भगवान् के द्वार अपने समक्ष खुलते हुए पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में वे सब बाह्य भेद जिन्हें मनुष्य इतना अधिक मानते हैं, क्योंकि वे बहिर्मुख मन को बरबस अपनी ओर खींचते हैं, भागवत् ज्योति की समता और पक्षपातरहित शक्ति की सर्वशक्तिमत्ता के सामने बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं।
जीवन में सबसे महत्त्वपूर्ण चीज है भगवान् की ओर जाना और जब उनके द्वार सभी के सामने समान रूप से खुले हैं तब फिर बाह्य भेदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, वे द्वार तो उनके लिए अधिक खुले हैं जो अकिंचन हैं, जिनके पास किसी प्रकार के कोई साधन नहीं हैं, जिनमें कोई क्षमताएँ नहीं हैं, जिनमें ज्ञानाभिमान नहीं है। इसी कारण भारतीय संस्कृति ने किसी के साथ भी कभी किसी प्रकार का भेदभाव किये बिना सभी के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि प्रत्येक प्राणी यथाशीघ्र अपने गंतव्य तक पहुँच सके। इसी दृष्टिकोण से हमारी सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाएँ और संस्थाएँ आदि विकसित हुईं ताकि वे इस उद्देश्य में अधिकाधिक सहायक हो सकें।
गीता में यहाँ इसी बात पर बल दिया गया है कि व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट क्यों न हों, व्यक्ति चाहे कितने भी निकृष्ट कुल में क्यों न पैदा हुआ हो, फिर भी भगवान् की भक्ति आने पर वह भी परम गति को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कोई दुराचारी भी यदि यह संकल्प कर ले कि भगवान् ही एकमात्र वरण करने योग्य हैं और इस कारण जो अपनी सारी शक्ति उसी ओर लगाता है, वह साधु मानने योग्य है और वह अपने पूरे कुल का कल्याण कर देता है, वहीं एक सात्विक ब्राह्मण, सभी नियमों आदि का पालन करते हुए भी, यदि भगवान् की भक्ति से शून्य है, तो अपने आप को भी मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए वास्तविक महत्त्व केवल भगवान् से लगाव का है। बिना भक्ति हुए न ज्ञान का कोई मूल्य है, न ही किन्हीं अनुभवों का। बिना भक्ति के ये सब वैसे ही हैं जैसे कि निष्प्राण देह पर आभूषण। यही नहीं, अहं के लिए उपयोग करने पर तो ये नुकसानदेह बन जाते हैं। व्यक्ति का उतना ही मूल्य है जितना वह भगवान् के प्रति समर्पित है, उसके अतिरिक्त उसका कोई भी मूल्य नहीं है। यदि यह मूलमंत्र समझ में आ जाए तो जीवन में यह व्यक्ति की अनेकों संकटों से रक्षा कर सकता है। अन्यथा तो संसार में इंद्रियों की तृप्ति, अपने अहं की तुष्टि आदि का इतना विष फैला हुआ है कि उससे बच पाना संभव नहीं है।
किं पुनर्बाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ।। ३३ ।।
३३. तो फिर पवित्र ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों का तो कहना ही क्या; इस अनित्य और दुःखमय लोक में आये हुए हे जीव! मेरी ओर अभिमुख हो और मेरी भक्ति कर।
यह पार्थिव जगत्, जो द्वन्द्वों में लिप्त है और जो घड़ी घड़ी के तात्कालिक क्षणिक सम्बन्धों से बँधा हुआ है, मनुष्य के लिए तब तक संग्राम, दुःख और शोक का ही जगत् है जब तक कि वह इन सब चीजों में ही आसक्त हुआ रहता है और इन्हीं के द्वारा लादे जानेवाले विधान को अपने जीवन का विधान मानता है। मुक्ति का मार्ग है बाह्य से हटकर अन्दर की ओर मुड़ना, भौतिक जीवन जो अपना भार मन पर लाद देता है और उसे प्राण और शरीर के खाँचों में कैद कर देता है - द्वारा रचित बाह्य प्रतीतियों से हटकर उस दिव्य सत्य अथवा यथार्थता की ओर मुड़ना जो आत्मा की मुक्तावस्था के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करने की प्रतीक्षा में है। संसार के प्रति प्रेम को, जो कि मुखौटा या मिथ्याप्रतीति है, भगवान् के प्रति प्रेम में रूपान्तरित होना होगा, जो कि सत्य है। एक बार जब इस गुप्त और अंतःस्थित ईश्वर को जान लिया जाता है तथा अंगीकार कर लिया जाता है तब सारी सत्ता और सारा जीवन एक श्रेष्ठ उत्थान और एक विलक्षण रूपान्तर की क्रिया से गुजरेगा। निम्नतर प्रकृति के अज्ञान की जगह, जो अपने बाह्य कर्मों और दृश्यों में निमग्न रहती है, दृष्टि सर्वत्रव्याप्त ईश्वर के दर्शन की ओर, आत्मा के ऐक्य और उसकी सार्वभौमिकता की ओर खुल जाएगी। संसार का दुःख-दर्द सर्वानन्द के आनन्द में खो जाएगा; हमारा दौर्बल्य, प्रमाद और पाप शाश्वत की सर्वालिंगनकारी और सर्व-रूपान्तरकारी शक्ति, सत्य और पवित्रता में परिवर्तित हो जायेगा।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ।। ३४।।
३४. मेरे चित्त वाला बन, मेरा प्रेमी और उपासक, मेरे प्रति यज्ञ करने वाला बन, मुझे नमस्कार कर, इस प्रकार आत्मा में मेरे साथ युक्त होकर, मुझे अपना परम ध्येय बनाकर, तू मेरे पास आ जाएगा।
मन को भागवत् चेतना के साथ एक करना, अपनी सम्पूर्ण भावावेगमय प्रकृति को सर्वत्र स्थित भगवान् के प्रति प्रेमरूप बना देना, अपने सब कर्मों को जगत्पति के प्रति एक यज्ञ बना देना और अपनी सारी उपासना और अभीप्सा को उनकी भक्ति तथा आत्मसमर्पण बना देना, सम्पूर्ण स्वत्व को समग्र ऐक्य में भगवान् की ओर लगा देना - यही सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर दिव्य जीवन को प्राप्त करने का मार्ग है। यही भागवत् प्रेम और भक्ति के सम्बन्ध में गीता की शिक्षा है, जिसमें ज्ञान, कर्म और हृदय की चाह सब परम एकत्व में एक हो जाते हैं, उनकी सारी विषमताएँ घुल-मिल जाती हैं, सब सूत्र आपस में गुँथ जाते हैं, एक महान् एकीकरण होता है, एक विस्तृत तादात्म्यकारी क्रिया होती है।
इस प्रकार नवाँ अध्याय 'राजविद्याराजगुह्मयोग' समाप्त होता है।
दसवाँ अध्याय
I. गीता का परम् वचन
अब हम गीता के योग के अंतरतम सारतत्त्व तक, उसकी शिक्षा से समस्त प्राणवंत और श्वास-प्रश्वास के केंद्र तक आ गये हैं। अब हम स स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं कि सीमित मानव जीव का अहंकार और निय प्रकृति से हटकर स्थिर, शान्त और अविकार्य अक्षर आत्मा में आ उसके आरोहण का केवल एक प्रथम सोपान, एक प्राथमिक परिवर्तन-भत्र था। और अब हम यह भी देख सकते हैं कि गीता ने आरम्भ से ही ईश्वर पा मानवरूप में परमेश्वर पर इतना बल क्यों दिया - उन परमेश्वर पर जो स्वयं को अहं, माम् आदि पदों से सूचित करते हैं, और उनका इस रूप में वर्णन है कि वे कोई महान् गुह्य और सर्वव्यापी परम सत्ता, जगतों के पति और माना आत्मा के नाथ हैं, वे जो उस अक्षर आत्मसत्ता से भी महान् हैं जो सदा शान और अचल रहती है और प्राकृत विश्व के अंतर्बाह्य (आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ) दृश्यों से निरन्तर अलिप्त बनी रहती है।
ये परम परमेश्वर सभी कुछ के एक ही अविकार्य अक्षर पुरुष हैं; इसलिए इस अविकार्य अक्षर पुरुष की आध्यात्मिक चेतना की ओर मनुष्य को जागृत होकर उसके साथ अपने अंतःस्थ निर्वैयक्तिक स्वरूप को एक करना होता है। मनुष्य में वे ही परमेश्वर हैं जो उसकी सब क्रियाओं का प्रवर्तन और संचालन करने वाले हैं; इसलिए मनुष्य को अपने स्वयं के इन अंतःस्थ ईश्वर के प्रति जागना, अपने अंदर निहित भगवत्-तत्त्व को जानना, जो कुछ उसे आच्छादित और प्रच्छन्न करता है उस सब से ऊपर उठ जाना और उसकी आत्मा को इस अन्तरतम आत्मा के साथ, अपनी चेतना की इस बृहत्तर चेतना के साथ अपने सारे संकल्प और कर्मों के इन गुप्त स्वामी के साथ, अपने अन्दर को इस परम सत्ता के साथ, जो उसके सारे विभिन्न भूतभावों का उद्गम और लक्ष्य है, एकीभूत होना होता है। ये ही वे परमेश्वर हैं जिनकी दिव्य प्रकृति, जो कि हम जो कुछ हैं उसका उद्गम है, इन निम्न प्राकृत विकारों से घने रूप से ढकी है; इसलिए मनुष्य को अपने निम्न बाह्य अस्तित्व, जो अपूर्ण और मत्वं है, से हट कर अपनी अमरता और पूर्णता वाली मूल दिव्य प्रकृति को पुनः प्राप्त करना होता है। ये परमेश्वर सब पदार्थों के अंदर एक हैं, वह आत्मा हैं जो सबके अन्दर रहती है और जिसके अन्दर सब रहते और गति करते हैं। इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों के साथ अपनी आत्मिक एकता ढूँढ़ निकालना, सब को उस एक आत्मा के अन्दर देखना और उस आत्मा को सबके अन्दर देखना, और यहाँ तक कि सब पदार्थों और प्राणियों को, आत्मौपम्येन सर्वत्र, सर्वत्र आत्मवत् देखना और तदनुसार अपने मन, बुद्धि और प्राण में सब में सोचना, अनुभव करना और कर्म करना होता है। ये ईश्वर यहाँ अथवा और कहीं जहाँ जो कुछ है उसके मूलस्रोत हैं और अपनी प्रकृति के द्वारा वे ये सब भूत बने हैं, अभूत् सर्वभूतानि, इसलिए मनुष्य को सब जड़ और चेतन पदार्थों में उन्हीं 'एक' को देखना और पूजना होता है; सूर्य में, नक्षत्र में, फूल में, मनुष्य और प्रत्येक जीव में, प्रकृति के सब रूपों और प्रभावों तथा गुणों और शक्तियों में 'वासुदेवः सर्वमिति' जानकर उनकी अभिव्यक्ति का पूजन करना होता है। उसे अपने-आप को दिव्य-दर्शन और दिव्य सहानुभूति के द्वारा और अन्ततः एक प्रबल आंतरिक तादात्म्य के द्वारा विश्व के साथ एक होकर विश्वमय होना होता है। एक निष्क्रिय संबंधरहित तादात्म्य प्रेम और कर्म को बाहर छोड़ देता है, किन्तु यह विशालतर और समृद्धतर एकत्व कर्मों के द्वारा तथा एक विशुद्ध प्रेमभाव के द्वारा अपने-आप को कार्यान्वित करता है: यह हमारे सभी कर्मों और भावनाओं का मूलस्रोत, आश्रय, सार, प्रेरक भाव और दिव्य प्रयोजन बन जाता है।... एक निष्क्रिय संबंधरहित तादात्म्य में आराधना और भक्ति का आनन्द नहीं रहता; परंतु भक्ति तो इस समृद्धतर, पूर्णतर और घनिष्ठतर ऐक्य की स्वयं आत्मा और मर्म और पराकाष्ठा ही है। ये भगवान् ही सभी संबंधों - पिता, माता, प्रेमी, सखा – की परिपूर्णता हैं और प्रत्येक प्राणी की आत्मा के आश्रय हैं। ये ही एकमेव परम और विश्वव्यापक देव, आत्मन्, पुरुष, ब्रह्म, गुप्त ज्ञान (उपनिषद्) के ईश्वर हैं। इन्होंने अपने अन्दर इन सब विभिन्न रूपों में अपने दिव्य योग के द्वारा जगत् को प्रकट किया हैः इसके अनेकविध भूतभाव इनके अन्दर एक हैं और ये उन सबके अन्दर अनेक पक्षों में एक हैं। इन सब रूपों में उनके प्राकट्य के प्रति जागृत होना ही उसी दिव्य योग' का मानवी पहलू है।
vi. 32, vii.19
______________________
* वही जग का निर्माता और स्वयं वह जगत् है जिसे उसने रचा है,
वही दर्शन है और वही द्रष्टा है;
वह स्वयं ही कर्ता और वही कर्म है,
वह स्वयं ही ज्ञाता है और वही ज्ञात है,
वह स्वयं ही स्वप्न-द्रष्टा है और स्वप्न है।
चूंकि हमारी सामान्य बहिर्मुख चेतना से श्रेष्ठतर चेतना में हमें इस प्रकार का दर्शन और अनुभव प्राप्त होता है कि सब कुछ वही है इसलिए वही सच्चा और यथार्थ दर्शन है और हमारी सामान्य चेतना का दर्शन त्रुटिपूर्ण या भ्रमित है। एक अधिक परिपक्व चेतना का दर्शन ही अधिक यथार्थ होता है। इसलिए भले ही वर्तमान में हमें अपनी अज्ञानमय चेतना के कारण स्वयं ऐसी अनुभूति न होती हो तो भी हमें इस मार्ग पर जा चुके उन अनगिनत ऋषियों-मुनियों, साधु-संन्यासियों की वाणी पर विश्वास करना होगा जो कि एक ही स्वर में इसी एक सत्य को दुहराते हैं कि सभी कुछ वे परमात्मा ही हैं उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। परंतु यदि सभी कुछ केवल वे परमात्मा ही हैं तो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम इम दृश्य जगत् में उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए जहाँ कहीं पी भगवान् के गुणों का विशिष्ट प्राकट्य होता है वहाँ हम उन्हें अधिक सरलता से पहचान सकते हैं। इसी के लिए भगवान् अर्जुन को विभूति योग का उपदेश करते हैं। हमारी संस्कृति में जिस किसी में और जहाँ कहीं भी भगवान् की सत्ता का अधिक प्राकट्य देखने को मिलता है उसे सदा ही विशिष्ट महत्त्व दिया जाता रहा है। आजकल के बुद्धिजीवियों के मुख से कई बार हम सुनते हैं कि हमें अपनी सारी योजनाएँ सबसे कमजोर और वंचित व्यक्ति के अनुसार बनानी चाहिये। परंतु ऐसा करना तो प्रकृति में अंतर्निहित आरोहण की प्रवृत्ति का ही खंडन करना हुआ। क्या हम अपना आदर्श भगवान् कृष्ण को न बनाकर किसी दीन-हीन, वंचित या प्रताड़ित व्यक्ति को बनाएँगे? इसीलिए गीता भगवान् को विभूति पर अत्यधिक बल देती है क्योंकि उसमें भगवान् की अभिव्यक्ति बिल्कुल प्रबल रूप से देखने को मिलती है। और यह विशिष्ट अभिव्यक्ति सभी चीजों में होती है, देवताओं, दानवों, पशुओं, मनुष्यों आदि में सब में उनकी विभूति हो सकती है। यही निरूपण अगले अध्याय में आएगा।
श्रीभगवान् उवाच
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।। १॥
१. श्रीभगवान् ने कहाः हे महाबाहो। अब मेरे परम वचन को सुन, जिसे मेरी आत्मा के कल्याण की इच्छा से कहूँगा, क्योंकि तेरा हृदय अब हमें अंदर आनन्द ले रहा है।
ऐसा पूर्ण रूप से और निर्विवाद रूप से स्पष्ट कर देने के लिए कि उनकी शिक्षा का यही परम और सम्पूर्ण अर्थ है, यही वह समग्र ज्ञान है, जिसे प्रकट करने का उन्होंने वचन दिया था, भागवत् अवतार अब तक जो कुछ कहते रहे हैं उसी के निष्कर्ष को सारांश रूप से दुहराते हुए यह बतलाते हैं कि, यही, और कोई नहीं, मेरा 'परमं वचः', परम वचन है।... हम पाते हैं कि गीता का यह परम वचन, प्रथमतः यही सुस्पष्ट और असंदिग्ध घोषणा है कि भगवान् क्की परमा भक्ति और परम ज्ञान उन्हें इस रूप में जानना और पूजना है कि वे, जो कुछ भी अस्तित्वमान है उसके, परम और दिव्य मूलस्रोत हैं और इस जगत् तथा इसके प्राणियों के सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हैं और सब पदार्थ जिनकी सत्ता के भूतभाव हैं। दूसरे, यह परम वचन एकीभूत ज्ञान और भक्ति को परम योग के रूप में घोषित करता है; यही सनातन पुरुष परमेश्वर के साथ मिलन लाभ करने का मनुष्य के लिए सुनिश्चित और स्वाभाविक मार्ग दिया गया है। और मार्ग के विषय में इस रूपरेखा को और भी अर्थपूर्ण बनाने के लिए, भक्ति को इस उच्चतम महत्ता को प्रदीप्त स्थान प्रदान करने के लिए... शिष्य के हृदय और मन द्वारा इसकी स्वीकृति को आगे आने वाले विस्तार के पहले एक शर्त के रूप में रखा गया है जिसमें अंततः मानव यंत्र अर्जुन को कर्म का अंतिम आदेश दिया जाना है। भगवान् कहते हैं, "मैं तेरी आत्मा के कल्याण की इच्छा से इस परम वचन को तुझसे कहूँगा, क्योंकि अब तेरा हृदय मेरे अन्दर आनन्द ले रहा है", ते प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। क्योंकि भगवान् में हृदय का यह आनन्द लेना ही सच्ची भक्ति का सम्पूर्ण घटक और सार है...
परम् वचन तभी दिया जा सकता है जब व्यक्ति को भगवान् में आनन्द आने लगे। यदि हृदय को भगवान् में कोई आनन्द ही न आ रहा हो तो उसे तो परम वचन दिया ही कैसे जा सकता है।
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २॥
२. न ही देवता और न ही महर्षिगण मेरी किसी उत्पत्ति के विषय में जानते हैं, मैं सर्वथा और हर प्रकार से देवताओं' का और महर्षियों का आदि कारण हूँ।
अतः, देवता परम पुरुष के माध्यम मात्र हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सृष्टि का निर्माण होता किस प्रकार है? सृष्टि हमारे लिए वैसी ही होती है जैसी हमारी चेतना होती है। पशु-पक्षियों को सृष्टि अपने तरीके से दिखाई देती है, मानव चेतना को सृष्टि पशु-चेतना से भिन्न प्रकार से दिखाई देती है। और मानव चेतना में भी व्यक्ति चेतना की श्रेणियों में किस स्तर पर स्थित है उस पर निर्भर करेगा कि उसे सृष्टि कैसी गोचर होगी। वैदिक शब्दावली के अनुसार जब व्यक्ति के यज्ञ का आरोहण होना आरंभ होता है, अर्थात् जब वह अपने निम्न भागों की अपेक्षा अधिकाधिक अपने उच्चतर भागों की क्रिया को स्थान देना आरंभ करता है, तो देवताओं की अर्थात् उसके अंदर निहित मनोवैज्ञानिक शक्तियों की अधिकाधिक समृद्धतर अभिव्यक्ति होने लगती है जिस कारण सृष्टि के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता जाता है। और ज्यों-ज्यों व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक शक्तियों की क्रिया अधिक प्रबल होती जाती है त्यों-ही-त्यों वह अधिक सशक्त रूप से क्रिया कर सकता है। उदाहरण के लिए, आवश्यक नहीं कि एक ऋषि में शारीरिक बल किसी आम व्यक्ति से अधिक हो, परंतु उसके अंदर अवश्य ही इतना प्रबल तेज और आध्यात्मिक शक्ति होती है कि उसके सान्निध्य में हिंसक पशुओं तक की प्रवृत्ति पर अंकुश लग जाता है और वहीं किसी मनुष्य की इतनी क्षमता नहीं होती कि सहज ही उसके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार कर सके। इसका कारण यह है कि उसके अंदर देवताओं की क्रिया अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक बिल्ली रहती तो उसी जगत् में है जिसमें हम रहते हैं, परंतु स्पष्ट ही है कि वह इस जगत् की भव्यताओं का कितना आनन्द ले पाती होगी। वेदों का मुख्य विषय ही यही है कि किस प्रकार हमारे अंदर के देवताओं को जागृत कर उनकी क्रिया को अधिकाधिक उन्नत कर दिया जाए। यही यज्ञ का आरोहण है। यहाँ भगवान् कह रहे हैं कि वे ही देवताओं के आदि कारण हैं और उनसे परे हैं। इस दृष्टिकोण से, जब हम भगवान् की चेतना में होते हैं तब हम प्रभुत्व का आस्वादन कर सकते हैं और जितने ही हम जड़तत्त्व से तदात्म होते हैं उतने ही हम नियम-विधानों में बँधे होते हैं। अतः सृष्टि अपने आप में और कुछ नहीं केवल हमारी चेतना के स्तर के अनुसार गोचर होती है। सांख्य शास्त्र ने तो पहले ही सारा विश्लेषण कर के हमें दिखा दिया कि भौतिक यथार्थता जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। सारी संरचना मनोवैज्ञानिक है। और जैसी हमारी संरचना होती है वैसी ही सृष्टि हमें गोचर होती है और वैसे ही नियम-विधान हमारे ऊपर लागू होते हैं। अतः, वस्तुतः अपने आप में कोई नियम नहीं हैं। चेतना जिस स्तर पर स्थित होकर अपनी क्रिया करती है उस स्तर के लिए वही नियमस्वरूप हो जाता है, हालाँकि उस स्तर के लिए अवश्य ही वह नियम बाध्यकारी होता है। और जब चेतना अत्यधिक ऊर्ध्वस्थित हो तब कोई बाहरी नियम बाध्यकारी नहीं होता, तब वह सर्वशक्तिमान होती है। अतिमानसिक चेतना में सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता होती है। भारतीय संस्कृति में सदा ही इसका भान रहा है। इसीलिए वे सदा ही चेतना के परिवर्तन पर बल देते थे क्योंकि वे जानते थे कि बाहरी फेर-बदल से वास्तव में कुछ भी संसिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी पाशविक चेतना के व्यक्ति के पास प्रचुर भौतिक सुख-साधन आदि हो सकते हैं परंतु फिर भी कला, साहित्य आदि गहरे विषयों का और उनसे मिलने वाली कहीं अधिक गहरी परितृप्ति का तो उसे कोई आभास तक भी नहीं हो सकता, न ही आत्मा के गहरे आनंदों का उसे लेशमात्र ही कोई आभास हो सकता है।
_________________________
* देवता महान् अमर शक्तियाँ और अमर व्यक्तित्व हैं जो विश्व की अंतर्बाह्य शक्तियों को सचेतन रूप से अनुप्राणित करते हैं, गठित करते हैं तथा उनकी अध्यक्षता करते हैं। देवता शाश्वत और आदिदेव के आध्यात्मिक रूप हैं जो उन आदिदेव से निकलकर जगत् की अनेक प्रणालियों में उतर आते हैं। देवता अनेकविध हैं, विश्वव्यापी हैं, वे आत्मसत्ता के मूलतत्त्वों और उसकी सहस्रों जटिलताओं के द्वारा उस 'एक' की ही वैविध्यपूर्ण सत्ता का संपूर्ण ताना-बाना निर्मित करते हैं। उनकी अपनी सारी सत्ता, प्रकृति, शक्ति, कर्मपद्धति हर तरह से, अपने एक-एक तत्त्व और अपनी बुनावट के एक-एक धागे में अनिर्वचनीय परात्पर के सत्य से ही निकलती हैं। यहाँ कुछ भी स्वतंत्र रूप से निर्मित नहीं होता, इन दिव्य माध्यमों (देवताओं) द्वारा कुछ भी आत्म-निर्भर रूप से नहीं किया जाता; सभी कुछ अपना मूल उद्गम, कारण, और अपनी सत्ता का और भूत-भाव का मूल आध्यात्मिक कारण चरम-परम परमेश्वर में पाता है…
इसलिए व्यक्ति कितना आनंद ले सकता है यह उसकी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। इससे बिल्कुल स्पष्ट ही है कि वास्तव में किसी संस्कृति का पूरा ध्यान किस चीज पर होना चाहिये। इसीलिए श्रीअरविन्द कहते हैं कि, "किसी महान् संस्कृति का संपूर्ण लक्ष्य होता है मानव को ऐसे कुछ तक उठा ले जाना जो वह आरंभ में नहीं हो, उसे ज्ञान तक ले जाना यद्यपि वह अथाह अज्ञान से प्रारंभ करता है, उसे उसके विवेक के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वास्तव में वह अधिकतर अपने अविवेक के द्वारा जीता है, शुभ एवं एकता के विधान के अनुसार (जीना सिखाना) भले ही वह अभी अशुभ और विषमता से भरा है. सौंदर्य एवं सामंजस्य के विधान द्वारा (जीना सिखाना) यद्यपि और कलहरत बर्बरता अस्तव्यस्तता ही हो, आत्मा के किसी उच्च विधान के द्वारा (जीती सिखाना) यद्यपि वर्तमान में वह अहंकारी, जड़, अनाध्यात्मिक, अपने सिखाना) यद्यपि आवश्यकताओं और कामनाओं द्वारा ग्रसित है। करि किसी सभ्यता का इनमें से कोई भी लक्ष्य न हो तो कदाचित् ही यह कहा जा सकता है कि उसकी कोई संस्कृति है, और किसी भी अर्थ में महान् और श्रेष्ठ संस्कृति तो निश्चित तौर पर नहीं (कहा जा सकता)। परंत इनमें से अंतिम लक्ष्य, जैसी कि प्राचीन भारत द्वारा कल्पना की गई थी, सभी (लक्ष्यों) से उच्च है क्योंकि वह अन्य सभी को समाहित करता है और अतिक्रम कर जाता है। यह प्रयत्न किया जाना जाति के जीवन को उदात्त बनाना है; इसमें असफल हो जाना भी इस बात से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जिसमें कि यह प्रयास किया ही न जाय; यहाँ तक कि इसमें आंशिक सफलता प्राप्त करना भी मानव की भावी संभावनाओं में महत् योगदान है।" (CWSA 20, 232)
जब कोई संस्कृति ऐसे विचारों और आदर्शों पर प्रतिष्ठित हो तब सहज ही है कि हर क्षेत्र में उसकी रचना और निर्माण का कोई सानी हो ही नहीं सकता क्योंकि तब कोई भी काम बोझ नहीं रह जाता अपितु वह तो आत्माभिव्यक्ति का, भगवान् के साथ संपर्क साधने का सर्वश्रेष्ठ साधन बन जाता है। जब कार्य के पीछे ऐसा उद्देश्य हो तब तो कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, गुणवत्ता आदि तो अद्भुत होंगे। यही भारतीय संस्कृति की अत्युत्कृष्ट उपलब्धियों का रहस्य रहा है। प्रत्येक क्रिया-कलाप को, प्रत्येक चीज को, प्रत्येक क्षण को चेतना के विकास का माध्यम बना दिया गया। यही यज्ञ है। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही बाहरी परिस्थितियाँ ज्यों की त्यों हों, फिर भी जैसे ही चेतना में परिवर्तन हो जाता है त्यों ही संपूर्ण सृष्टि बिल्कुल भिन्न रूप से गोचर होती है। श्रीअरविन्द व श्रीमाँ जिन जगतों में निवास कर रहे थे और जिस प्रकार की अनेक स्तरीय क्रिया कर रहे थे उसका तो उनकी बाहरी परिस्थितियों से हम कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इसलिए, सृष्टि वैसी ही होगी जैसी हमारी चेतना होगी।
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।
असंमूढः स मत्र्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। ३।।
३. जो कोई मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त जगतों और जीवों के शक्तिशाली प्रभु के रूप में जानता है, वह मृत्युशील मनुष्यों में मोहरहित होकर जीता है और समस्त पाप और अशुभ से मुक्त हो जाता है।
बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ।। ४।।
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ।। ५।।
४-५. बुद्धि, ज्ञान, अज्ञानजन्य मोह से मोक्ष, क्षमा, सत्य, आत्म-संयम, शांतचित्तता, सुख और दुःख, उत्पत्ति और विनाश, भय और अभय, यश और अपयश, अहिंसा, समता, सन्तोष, तप और दान, ये सब प्राणियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के मानसिक भाव हैं, और ये सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं।
भगवान् का वह भाव जिस पर गीता जीवन के संपूर्ण मर्म के गूढ़ रहस्य के रूप में, मोक्षदायी ज्ञान के रूप में आग्रह करती है, वह ऐसा है जो कालगत वैश्विक गति और विश्वातीत शाश्वतता के बीच के भेद को पाट देता है, और ऐसा वह इनमें से किसी भी एक को अस्वीकार किये बिना या किसी के सत्य में से कोई अंश निकाले बिना (उसके सत्य को कोई हानि पहुँचाए बिना) ही करता है। अपितु यह तो हमारी आध्यात्मिक धारणा और आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वेश्वरवादी (pantheistic), ईश्वरवादी (theistic) तथा सर्वोच्च विश्वातीत (transcendental) विषयों को समन्वित करता है। भगवान् अजन्मा शाश्वत हैं जिनका कोई उद्गम नहीं, उनसे पूर्व में न कुछ ऐसा है और न हो हो सकता है जिससे वे उद्भूत हुए हों, क्योंकि वे एक, कालातीत और परम निरपेक्ष हैं। "न ही देवता और न ही महर्षिगण मेरी कोई उत्पत्ति जानते हैं... जो मुझे अजन्मा अनादि जानता है..." इत्यादि इस परम वचन के प्रारंभिक कथन हैं.. विश्वातीत अनन्त की यह आध्यात्मिक अनुभूति जागतिक जीवन के विषय में सर्वेश्वरवादी धारणा की सीमाओं को तोड़ डालती है। एक विश्वमय-एकेश्वरवाद की अनंतसंबंधी धारणा, जो विश्व और ईश्वर को एक कर देती है, वह ईश्वर को उनकी जगत् अभिव्यक्ति में कैद करने का प्रयास करती है और इस जगत् अभिव्यक्ति को ही ईश्वर को जानने का एकमात्र संभव साधन रख छोड़ती है; परन्तु यह परम ज्ञानानुभूति हमें देश-कालातीत शाश्वत स्वरूप में मुक्त कर देती है। "आपके आविर्भाव को न देवता जानते हैं न असुर ही," यही अपने उत्तर में अर्जुन कह उठता है: यह सारा जगत् अथवा ऐसे असंख्य जगत् भी उन्हें प्रकट नहीं कर सकते, उनकी अनिर्वचनीय ज्योति और अनन्त महत्ता को धारण नहीं कर सकते। ईश्वर सम्बन्धी इससे कनिष्ठ कोटि के ज्ञान से परम् पुरुष परमेश्वर के चिर अव्यक्त और अनिर्वचनीय सत्स्वरूप पर आत होने के कारण ही सत्य हैं।
परन्तु साथ ही, दिव्य परात्पर विश्व का निषेध नहीं है, न ही यह को ऐसा परम निरपेक्ष है जो विश्व के साथ किसी भी सम्बन्ध से रिक्त हो। यह एक परम सकारात्मक अथवा वास्तविक तत्त्व है, सब निरपेक्षों का निरपेक्ष है। सभी विश्वगत सम्बन्ध इन्हीं परम से निकलते हैं; विश्व के सभी भूत इन्हीं के पास लौट जाते हैं और केवल इन्हीं में अपना सच्चा और अपरिमेय अस्तित्व लाम करते हैं। "क्योंकि मैं सर्वथा और हर प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि-कारण हूँ।"...
हमारे अस्तित्व के ये परम परात्पर मूल हमसे किसी ऐसी खाई द्वाग पृथक् नहीं हैं जिसे मिलाया न जा सके और न वे इन प्राणियों को, जो उन्हीं से निकले हैं, अपनी सन्तान मानने से इन्कार करते हैं और न इन सब को एक भ्रम की सृष्टि बताकर इन्हें दण्ड का भागी बताते हैं। वे ही परम सत्ता है और सब उन्हीं के भूतभाव हैं। वे कोई शून्य में से, किसी अभाव में से वा स्वप्न-रूप मिथ्यात्व में से सृजन नहीं करते। वे अपने-आप में से सृजन करते हैं, अपने अन्दर ही वे उत्पन्न होते हैं; सभी उन्हीं की सत्ता में विद्यमान हैं और सब कुछ उन्हीं की सत्ता का तत्त्व है। यह सत्य पदार्थों को देखने की जो सर्वेश्वरवादी दृष्टि है उसे स्वीकार करते हुए उसका अतिक्रमण कर जाता है। वासुदेवः सर्वम्, वासुदेव ही सब कुछ हैं, क्योंकि जगत् में जो प्रकट है वह सब वासुदेव ही है, और वासुदेव वह सब भी हैं जो जगत् में प्रकट नहीं है तथा वह सब भी जो कभी व्यक्त नहीं होता। उनकी सत्ता किसी प्रकार भी उनके भूतभाव या अभिव्यक्ति से सीमित नहीं है; इस सापेक्ष जगत् से वे किसी अंश में भी बँधे नहीं हैं। सभी कुछ बन जाने पर भी वे परम परात्पर ही हैं; सीमित रूपों को धारण करते हुए भी वे सदा अनन्त ही बने रहते हैं।...
श्रीअरविन्द इस चीज की व्याख्या कर रहे हैं कि आखिर वह परम वचन क्या है जो भगवान् अर्जुन को दे रहे हैं चूंकि अब उसका हृदय उनमें रस लेने लगा है। यदि हृदय को भगवान् में रस ही न आता हो तब तो उसे भगवान् के किसी स्वरूप का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भगवान् में आनंद आने पर ही उनका स्वरूप हमारे समक्ष प्रकट किया जा सकता है।
यहाँ परमात्मा के तीन भावों को अर्थात् ईश्वर भाव, सर्वेश्वर भाव और परात्पर भाव को समन्वित किया गया है। ये भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं जिनके आधार पर हम ईश्वर और इस जगत् के बीच के संबंध को परिभाषित और निर्धारित करते हैं। इस्लाम आदि सेमेटिक धर्म ईश्वरवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर इस जगत् से ऊपर स्थित हो सारी सृष्टि को शासक के रूप में चलाते हैं और इस जगत् में हम उन ईश्वर के बन्दे हैं। परम सत्ता और जगत् के साथ उनके संबंध के विषय में यह एक दृष्टिकोण है जो कि अपने आप में यथार्थ अनुभव है, परंतु है एक आंशिक अनुभव ही। दूसरा दृष्टिकोण सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण है जो कहता है कि सभी कुछ परमात्मा ही है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बहुत ही मुक्तिकारक तो है परन्तु गलत रूप से प्रयुक्त किये जाने पर इसके आधार पर हम बहुत सी मूर्खताएँ की जाती देखते हैं। सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण में व्यक्ति एक मानसिक धारणा बना बैठता है कि सब कुछ परमात्मा ही हैं, जो कि मूलतः एक सत्य है, परंतु इसका मानसिक निरूपण एक सीमा के बाद मिथ्या हो जाता है क्योंकि संसार में वैविध्य है और सभी के साथ व्यवहार करना आवश्यक है। इसलिए गलत रूप से प्रयुक्त करने पर तो व्यवहार करने का आधार ही नहीं रहता। यही बात तो हमें हाथी और महावत की प्रचलित कथा से स्पष्ट होती है। आजकल के प्रचलित समानता आदि के विचार भी इसी दृष्टिकोण से प्रभावित हैं परंतु पुनः, समानता आदि के विचार ऐसे मूलभूत सत्य हैं जिन्हें कि यदि बाहरी रूप से प्रयुक्त करने का प्रयास किया जाए तो बड़े ही भयंकर परिणाम भी आ सकते हैं। जितना ही हम बाहरी रूप से समानता लाने का प्रयास करते हैं उतनी ही विषमताएँ बढ़ती जाती हैं क्योंकि समानता बाहरी चीजों से निर्धारित नहीं की जा सकती। व्यक्ति के आंतरिक गठन के अनुसार उसके साथ व्यवहार करने पर ही सच्चे रूप से समान व्यवहार किया जा सकता है। जब कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हैं तब उनके साथ समानता के किन्हीं भी मानदंडों के अनुसार व्यवहार कैसे किया जा सकता है। इसीलिए, सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण भी एक मूलतः सही अनुभव है परंतु बहुत बार व्यवहार के अंदर जिस रूप में इसे प्रयुक्त किया जाता है उससे बहुत सी विषमताएँ उठ खड़ी होती हैं। सर्वेश्वरवादी के दृष्टिकोण से सभी कुछ परमात्मा स्वयं ही हैं। यह बात मूलतः तो सही है परंतु फिर क्या एक पत्थर और एक मनुष्य में चेतना की समान ही अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है?
यदि हम ईश्वरवादी दृष्टिकोण को किसी ऐसी अपूरणीय खाई से न बाँट दें जिसमें कि ईश्वर और उनकी सृष्टि का आपस में कोई मिलन संभव ही न हो, तो इस जगत् में हमें भगवान् की उत्तरोत्तर वर्धित होती हुई अभिव्यक्ति गोचर होती है। कदाचित् ही कोई इस बात से इंकार करेगा कि पत्थर अथवा पशु-पक्षियों में ईश्वर की जितनी अभिव्यक्ति होती है उससे कहीं श्रेष्ठतर अभिव्यक्ति मनुष्य में है। और यदि हमारे अंदर थोड़ा भी विवेक हो तो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि स्वयं मनुष्यों में भी उत्तरोत्तर वर्धित होती चेतना की श्रृंखला है।
सनातन धर्म में ऐसी कोई अपूरणीय खाई कभी नहीं खींची गई। सनातन धर्म के अंदर सदा ही परमात्मा को अधिकाधिक वर्धमान अभिव्यक्ति को स्वीकार किया जाता रहा है। एक महापुरुष अथवा एक संत किसी सामान्य मनुष्य से अधिक परमात्मा को अभिव्यक्त करते हैं। एक विभूति उससे कहीं अधिक अभिव्यक्त करती है और एक अवतार तो भगवान् की और भी अधिक अभिव्यक्ति करते हैं। जब हम इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं तो सहज ही हम जहाँ भगवान् की अधिक अभिव्यक्ति पाते हैं उसके प्रति नतमस्तक हो सकते हैं। इसीलिए गुरु के प्रति, एक विभूति के प्रति या फिर एक अवतार के प्रति नतमस्तक होना, उसके प्रति श्रद्धा रखना आत्मोत्थान का एक बड़ा ही शक्तिशाली तरीका है। इसलिए यदि इस दृष्टिकोण को सही रूप से लिया जाए तो यह हमें विभूतियोग से जोड़ देता है। विभूतियोग का उपदेश करते हुए भगवान् साथ में यह भी कहते हैं कि सारे ब्रह्माण्ड भी उनसे निःसृत एक चिनगारी मात्र ही हैं जबकि वे स्वयं तो इस सब को अतिक्रम कर जाते हैं। वास्तव में परमात्मा हमारे किन्हीं भी ऊँचे से ऊँचे मानसिक निरूपणों को सर्वथा अतिक्रम कर जाते हैं। हमारे वेद भी उस तत्त्व का निरूपण करने के बाद 'नेति, नेति' ही कहते हैं अर्थात् परमात्मा इन किन्हीं भी चीजों से बढ़ नहीं होते बल्कि सभी कुछ से परे होते हैं, यहाँ तक कि वे असीमितता से भी बद्ध नहीं हैं। वे सीमित हो जोते हैं और इन दोनों से (सीमितता और असीमितता से) परे भी हैं और नहीं भी हैं। सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण जो भगवान् व जगत् का एकत्व मानता है एक तरह से भगवान् को सीमित कर देता है व उनके परात्पर रूप के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। इस प्रकार ईश्वर के ये तीन भाव हैं। हालाँकि ये तीनों परस्पर एक दूसरे से विरोधात्मक प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में ये ऐसे हैं नहीं। परंतु चूंकि
यदि हम ईश्वरवादी दृष्टिकोण को किसी ऐसी अपूरणीय खाई से न बाँट दें जिसमें कि ईश्वर और उनकी सृष्टि का आपस में कोई मिलन संभव ही न हो, तो इस जगत् में हमें भगवान् की उत्तरोत्तर वर्धित होती हुई अभिव्यक्ति गोचर होती है। कदाचित् ही कोई इस बात से इंकार करेगा कि पत्थर अथवा पशु-पक्षियों में ईश्वर की जितनी अभिव्यक्ति होती है उससे कहीं श्रेष्ठतर अभिव्यक्ति मनुष्य में है। और यदि हमारे अंदर थोड़ा भी विवेक हो तो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि स्वयं मनुष्यों में भी उत्तरोत्तर वर्धित होती चेतना की श्रृंखला है।
सनातन धर्म में ऐसी कोई अपूरणीय खाई कभी नहीं खींची गई। सनातन धर्म के अंदर सदा ही परमात्मा को अधिकाधिक वर्धमान अभिव्यक्ति को स्वीकार किया जाता रहा है। एक महापुरुष अथवा एक संत किसी सामान्य मनुष्य से अधिक परमात्मा को अभिव्यक्त करते हैं। एक विभूति उससे कहीं अधिक अभिव्यक्त करती है और एक अवतार तो भगवान् की और भी अधिक अभिव्यक्ति करते हैं। जब हम इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं तो सहज ही हम जहाँ भगवान् की अधिक अभिव्यक्ति पाते हैं उसके प्रति नतमस्तक हो सकते हैं। इसीलिए गुरु के प्रति, एक विभूति के प्रति या फिर एक अवतार के प्रति नतमस्तक होना, उसके प्रति श्रद्धा रखना आत्मोत्थान का एक बड़ा ही शक्तिशाली तरीका है। इसलिए यदि इस दृष्टिकोण को सही रूप से लिया जाए तो यह हमें विभूतियोग से जोड़ देता है। विभूतियोग का उपदेश करते हुए भगवान् साथ में यह भी कहते हैं कि सारे ब्रह्माण्ड भी उनसे निःसृत एक चिनगारी मात्र ही हैं जबकि वे स्वयं तो इस सब को अतिक्रम कर जाते हैं। वास्तव में परमात्मा हमारे किन्हीं भी ऊँचे से ऊँचे मानसिक निरूपणों को सर्वथा अतिक्रम कर जाते हैं। हमारे वेद भी उस तत्त्व का निरूपण करने के बाद 'नेति, नेति' ही कहते हैं अर्थात् परमात्मा इन किन्हीं भी चीजों से बढ़ नहीं होते बल्कि सभी कुछ से परे होते हैं, यहाँ तक कि वे असीमितता से भी बद्ध नहीं हैं। वे सीमित हो जोते हैं और इन दोनों से (सीमितता और असीमितता से) परे भी हैं और नहीं भी हैं। सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण जो भगवान् व जगत् का एकत्व मानता है एक तरह से भगवान् को सीमित कर देता है व उनके परात्पर रूप के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। इस प्रकार ईश्वर के ये तीन भाव हैं। हालाँकि ये तीनों परस्पर एक दूसरे से विरोधात्मक प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में ये ऐसे हैं नहीं। परंतु चूंकि हमारे मन की अपनी सीमाएँ हैं और वह समग्रता में किसी चीज को नहीं देख सकता इसलिए किसी एक दृष्टिकोण को अपनाकर इस पर आग्रह करता है कि वही एकमात्र सच्चा दृष्टिकोण है।
वास्तव में हमारा मन ज्ञान का उपकरण नहीं है। इसलिए ज्ञान के लिए इसका उपयोग करना अनुचित है। मन के कार्य के विषय में श्रीमाताजी कहती हैं, "...मन का सच्चा कार्य है कर्म की रचना करना और व्यवस्थापन करना। मन में एक रचनात्मिका और संगठनकारी शक्ति है, और यही वह चीज है जो कर्म के उद्देश्य से, कर्म की व्यवस्था के लिये अंतःप्रेरणा के विभिन्न तत्त्वों को यथाक्रम रखती है। और मन अपने आप को इसी भूमिका तक सीमित रखे, अंतःप्रेरणाओं को ग्रहण करे - वे चाहे ऊपर से आयें अथवा अंतरात्मा के गुह्य केंद्र से - और केवल कर्म की योजना का निर्माण करे (चाहे विस्तीर्ण रूप-रेखा के साथ या अत्यंत छोटे-छोटे ब्यौरों के साथ, चाहे जीवन की लघुतम बातों के लिये या महान् विश्व-व्यवस्था के लिये), तो वह अपने कार्य को पर्याप्त रूप से पूरा करेगा।
यह ज्ञान का उपकरण नहीं है।
परंतु वह कर्म के लिये, कर्म की व्यवस्था के लिये ज्ञान का उपयोग कर सकता है। यह सुव्यवस्था और रचना का एक उपकरण है और यह जब सुविकसित होता है तो बहुत शक्तिशाली और बहुत सुयोग्य उपकरण होता है।
मनुष्य, जब अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना चाहता है उदाहरणार्थ, अपनी सत्ता के अंदर विभिन्न तत्त्वों को उनके स्थान पर रखना चाहता है तो वह इस बात को बहुत स्पष्ट रूप में अनुभव कर सकता है। एक ऐसी विशेष बौद्धिक क्षमता है जो एकाएक प्रत्येक वस्तु को उसके स्थान पर रख देती है तथा एक योजना बना लेती और व्यवस्था कर लेती है। और वह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मन से आता है, वह एक ऐसा ज्ञान है जो, जैसा कि मैंने कहा है, आत्मा की गुह्य गहराइयों में से अथवा एक उच्चतर चेतना से आता है; और मन उसे भौतिक जगत् में एकाग्र करता तथा उच्चतर चेतना को कर्म का आधार देने के लिये उसे व्यवस्थित करता है।
मनुष्य को यह अनुभव उस समय बहुत स्पष्ट रूप में होता है जब वह अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहता है।
और फिर, इसका अन्य एक उपयोग भी है। मनुष्य जब अपनी तर्क-बुद्धि के, बुद्धि के तर्कशील केंद्र के, विशुद्ध तर्क-बुद्धि के संपर्क में होता है तो समस्त प्राणिक आवेगों के ऊपर यह एक शक्तिशाली नियंत्रण होता है। जो कुछ प्राण-जगत् से आता है उस पर उसके द्वारा बहुत दृढ़ता के साथ संयम प्राप्त किया जा सकता और उसे नियंत्रित और व्यवस्थित कर्म में प्रयुक्त किया जा सकता है। परंतु उसे किसी अन्य वस्तु की सेवा में संलग्न होना चाहिये - न कि स्वयं की तुष्टि में।
ये ही मन के दो उपयोग हैं: यह एक नियंत्रणकारी शक्ति है, नियंत्रण करने का साधन है, और यह व्यवस्था करने की एक शक्ति है। वहीं इसका सच्चा स्थान है।" (CWM 5, 107-09)
इस प्रकार मन का एक तय दायरा है और अपनी एक सीमित उपयोगिता है परंतु यदि हम यह भ्रम कर बैठें कि हम संसार को, उसकी क्रिया को, उसके तौर-तरीकों को, भौतिक, प्राणिक और मनोवैज्ञानिक नियमों को उसके माध्यम से समझ गए हैं तो इससे बड़ी भारी भूल कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपनी मन-बुद्धि के माध्यम से जो नियम-विधान प्रतीत होते हैं वे तो केवल एक प्रतीति मात्र ही हैं। केवल एक चेतना विशेष पर रहने पर उसकी क्रियाविधि हमें नियमस्वरूप प्रतीत होती है। परंतु चेतना के उस स्तर को अतिक्रम करने पर या फिर चेतना के एक उच्चतर स्तर के विधान को निम्नतर स्तर पर सक्रिय करने पर वे ही नियम बाध्यकारी नहीं रहते और तब जिसे हम चमत्कार कहते हैं वे संभव हो जाते हैं। मनुष्य की चेतना में जो चीजें सहज होती हैं वे संभवतः पशु की चेतना के लिए चमत्कार प्रतीत होती हों, वहीं मनुष्य को देवताओं की क्रिया चमत्कारिक प्रतीत होती है। अतः चेतना के स्तर पर निर्भर करता है कि प्रकृति और पुरुष का परस्पर संबंध क्या होगा। चेतना का स्तर जितना ऊँचा होगा प्रकृति पुरुष की इच्छा के प्रति उतनी ही नमनीय होगी।
इसलिए गीता यहाँ हमारे समक्ष ईश्वर के विभिन्न भावों को प्रकट कर रही है ताकि हमारी बुद्धि में यह पर्याप्त नमनीयता आ सके कि किस प्रकार परमात्मा एक साथ सभी भावों को अपनाने में सक्षम हैं और फिर भी वे स्वयं इन सभी से परे हैं। अतः हमें समझना होगा कि सभी कुछ के अंदर ईश्वर विद्यमान हैं परंतु इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि सब में विद्यमान होते हुए भी उनकी उत्तरोत्तर वर्धित अभिव्यक्ति है जिसके कारण हमें सभी के साथ उस अभिव्यक्ति के अनुसार यथायोग्य ही व्यवहार करना होगा। इसलिए सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण के साथ ही साथ वर्धित होती अभिव्यक्ति के नियम का भी सम्मान रखना होगा जिससे कि सभी मूलतः भगवान् होते हुए भी हम व्यवहार में एक पत्थर और एक मनुष्य के साथ, एक सामान्य मनुष्य और एक संत के साथ, एक संत और एक विभूति के साथ यथोचित व्यवहार कर सकें। और इन सब के साथ ही साथ यह भान भी आवश्यक है कि भगवान् अपनी किन्हीं भी अभिव्यक्तियों से सीमित नहीं हो सकते। वे तो इन सबसे परे भी हैं, परात्पर हैं। यदि इन सब भावों को हम एक साथ समन्वित कर सकें तभी हम सही रूप से देख पायेंगे अन्यथा सदा ही आशंका बनी रहती है कि हम किसी भी एक सूत्र में बंध जाएँगे और परमात्मा के दूसरे पक्ष को चूक जायेंगे।
यह सीमित बाह्य भूतभाव दिव्य अनन्त को व्यक्त करनेवाला एक प्राकृत भाव है।....और इस निम्न, बाह्य और प्रतीयमान व्यवस्था-क्रम में प्रकृति, जो भगवान् के व्यक्त होने की एक शक्ति है, वह तमसाच्छन्न वैश्व अज्ञान की विकृतियों से विरूपित हो जाती है और उसके दिव्य माहात्म्य या महत्त्व हमारी मानसिक और प्राणिक अनुभूति की जड़-स्थूल, विभाजक और अहंकारमय प्रक्रिया में लुप्त हो जाते हैं। पर तो भी, यहाँ भी जो कुछ है, चाहे जन्म हो या संभूति हो या विकास हो, सब परम् पुरुष परमेश्वर से ही है, एक विकास-क्रम है जो परात्पर से निकली हुई प्रकृति की क्रिया द्वारा होता है। भगवान् कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अर्थात् "मैं ही सभी कुछ की उत्पत्ति हूँ और मुझसे ही सब कुछ कर्म और गतिरूप विकास में प्रवृत्त होता है।" यह बात केवल उस सब के लिए ही सही नहीं है जिसे हम शुभ कहते हैं या जिसकी प्रशंसा करते हैं तथा जिसे हम दिव्य मानते हैं, वह सब जो ज्योतिर्मय, सात्त्विक, सदाचारयुक्त, शान्तिप्रद, आत्मिक रूप से आनन्दप्रद है....ऐसा उन विपरीत भावों के लिए भी सच है जो मर्त्य मन को व्याकुल कर देते हैं और अज्ञान और उसका संभ्रम ले आते हैं, प्रकाश और अंधकार की परस्पर शेष सभी क्रीड़ाओं के साथ, "दुःख और सुख, जन्म और मृत्यु, भय और अभय, यश और अपयश" ले आते हैं....
x.8
प्रश्न : पर जो तानाशाह हजारों लोगों को मार डालते हैं, या फिर जो आतंकवादी आतंक फैलाते हैं वे सब भी तो बिना भगवान् की इच्छा के भगवान् को ऐसी चीजों इच्छा होती है ?
उत्तर : यह एक बड़ा ही जटिल प्रश्न है जो कि बहुत ही आप है परतु यह उठता है मन के एकांगी स्वरूप के कारण। अब एक उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से हम कुछ-कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। हालाँकि वास्तव में तो कोई भी उदाहरण कभी भी पूर्ण रूप से सटीक नहीं हो सकता क्योंकि जिन भी रूपकों आदि का हम प्रयोग करते हैं वे कभी भी परम सत्य को परिभाषित नहीं कर सकते। फिर भी इस सबसे बुद्धि के लिए विषय को समझना कुछ अधिक सुगम हो जाता है। अब मान लीजिये कि आप ही के घर में, आप ही की ताश से आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि खेल में सबके पास जो अच्छे या बुरे पत्ते आ रहें हैं वे सब आप की ही मर्जी से आ रहे हैं। इसीलिए भले ही सब में परमात्मा व्याप्त हैं तो भी भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं अर्जुन को युद्ध में सब को मार डालने के लिए कह रहे हैं। समस्या मूलभूत सत्य में नहीं है, अपितु हमारे सीमित व संकीर्ण दृष्टिकोण में है जो केवल एक सीधी रेखा में ही देख सकता है जबकि वह सत्य तो अनंत आयामी है इसलिए जब हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान् की ही इच्छा से होता है तो मूलतः तो यह बात सत्य है परंतु इसे व्यवहार में प्रयुक्त करने में हम धोखा खा जाते हैं। कोई चीज घटित हो जाने के बाद तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ संभव था वही घटित हुआ है परंतु उससे पूर्व हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसके अंदर सदा ही हमारे व्यक्तिगत चयन की, विवेक की, हमारे हस्तक्षेप की संभावना रहती है। इसीलिए हमारी उच्चतम संभव चेतना के अनुसार हमारा व्यक्तिगत चयन बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो कि भावी संभावनाओं में अपना योगदान करता है। यदि ऐसा न होता और सब कुछ अपनी पूर्णत्व की ही स्थिति में होता तब तो किन्हीं अवतारों के अवतरण को और उनके हस्तक्षेप की भी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए भले ही अपने आप में कितने भी सापेक्ष क्यों न हों पर इस पार्थिव अभिव्यक्ति में सत्य के साथ असत्य भी है, मिथ्यात्व है, बुराई है, आदि भी हैं। हमारे वेदों, पुराणों आदि सभी सद्ग्रन्थों में हम यही बात पाते हैं। सभी पुराणों में हम राक्षसों के संहार की कथाएँ पाते हैं। वेदों में हम दुःख कष्ट-यंत्रणा वृत्रों और पणियों आदि निम्नतर वृत्तियों को नष्ट करने की बात पाते हैं। तो क्या हमारे वैदिक ऋषियों को यह सामान्य ज्ञान भी नहीं था कि सभी कुछ भगवान् से ही उत्पन्न होता है इसलिए उन्हें मारना नहीं चाहिये? अतः यह एक अनुत्पादक और अनुपयोगी विचार है कि सब कुछ भगवान् की ही इच्छा से हो रहा है। इससे हमें व्यावहारिक रूप से कोई सहायता या दिशानिर्देश प्राप्त नहीं होता।
स्वयं श्रीअरविन्द का सावित्री ग्रंथ इसी चीज को तो सामने लाता है। नारद जी ने सावित्री का भविष्य देख कर पहले ही यह घोषणा कर दी कि एक साल बाद सत्यवान् की मृत्यु निश्चित है। अब यदि सावित्री इसे स्वीकार कर लेती तो क्या कभी मृत्यु पर विजय संभव हो पाती। वास्तव में मानसिक रूप से अपनाया यह दृष्टिकोण कि सब कुछ भगवान् की ही मर्जी से होता है, एक बड़ा ही भगवद्विरोधी दृष्टिकोण है। क्योंकि ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसे कि अपने अनुकूल-प्रतिकूल, सुखद-दुःखद आदि अनुभव न होते होंगे। अतः पीड़ादायक अनुभवों में व्यक्ति यह विचार कर सकता है कि वह पीड़ा श्रीमाताजी की इच्छा से ही आई है और वे मनचाहे रूप से हमें दुःख और यंत्रणा में से गुजारती हैं। और ऐसे भाव से व्यक्ति का भगवान् से जुड़ाव समाप्त होने की आशंका रहती है। इसीलिए श्रीमाताजी साधकों को अनेक बार इस विषय में चेताती थीं कि ऐसी किन्हीं भी मानसिक धारणाओं को भगवान् पर थोपने का प्रयास न करें क्योंकि उसके बड़े ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कोई भी एकांगी दृष्टिकोण अपनाते ही हम अपने आप को भारी भूलों के प्रति खोल देते हैं क्योंकि यह एक ऐसा सत्य है जिसका केवल आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा ही बोध हो सकता है, मानसिक रूप से नहीं। और व्यावहारिक रूप से क्या करना चाहिये इसका भी व्यक्ति को अपने भीतर से निर्देश या इसकी प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए श्रीमाताजी कहती हैं कि व्यक्ति को अपनी उच्चतम संभव चेतना के स्तर से क्रिया करनी चाहिये तभी जो सर्वोत्तम है, वह होता है।
गीता परम सत्ता और उसके भूतभाव को स्वीकार करती है और उनके परस्पर अंतर को महत्त्व देती है, पर इसे कोई परस्पर विरोध में नहीं बदल देती। क्योंकि ऐसा करना तो विश्व के एकत्व का ही अभिनिषेध करना हुआ। भगवान् अपनी परात्परता में एक हैं, सभी पदार्थों के सर्व-धारक एक अखण्ड आत्मा हैं, अपनी विश्वप्रकृति के एकत्व में एक हैं। ये तीनों एक ही भगवान् हैं; सब कुछ उन्हीं से निकलता है, सब कुछ उन्हीं की सत्ता से उत्पन्न होता है, सब कुछ उन्हीं का नित्य अंश अथवा अभिव्यक्ति है। यदि हमें गीता का अनुकरण करना है तो हमें भगवान् की उस परा स्थिति में, उप परम निरपेक्ष सत्ता में सब पदार्थों के किसी परम निषेध को नहीं अपितु उनके रहस्य की वास्तविक कुंजी को, उनके अस्तित्व के समन्वयकारी रहस्य को खोजना होगा।
परन्तु अनन्त सत्ता का एक और सत्स्वरूप है जिसे भी मोक्षप्रद ज्ञान के एक अपरिहार्य तत्त्व के रूप में जान लेना आवश्यक है। वह स्वरूप है भागवत शासन (भगवान्) का अपनी परा स्थिति से नीचे जगत् की ओर देखना और साथ ही जगत् में अंतर्यामी रूप से अपनी घनिष्ठ उपस्थिति बनाए रखना। जो परम् पुरुष समस्त सृष्टि बनते हैं और फिर भी उसे अनन्त रूप से अतिक्रम किये रहते हैं, वे जगत् के कोई ऐसे संकल्परहित आदि कारण नहीं हैं जो अपनी सृष्टि के विषय में उदासीन हों।..... वे सब भुवनों और उनके अधिवासियों के महाशक्तिशाली परमेश्वर, 'लोकमहेश्वर' हैं और सभी कुछ का केवल अन्दर से नहीं अपितु ऊपर से, अपनी परमातीत स्थिति से शासन करते हैं।
विश्व का शासन कोई ऐसी शक्ति नहीं कर सकती जो विश्व के परे न हो। भागवत् शासन का अर्थ ही है किसी सर्वशक्तिमान् शासक की मुक्त प्रभुता, न कि किसी सीमित अभिव्यक्ति की कोई स्वतःचालित शक्ति या यांत्रिक नियम जो विश्व की दृश्य प्रकृति से सीमित हो। यह विश्व के विषय में ईश्वरवादी दृष्टि है, परंतु यह कोई भयविकंपित या सशंक ईश्वरवाद नहीं है जो जगत् के द्वन्द्रों अथवा अंतर्विरोधों से भयभीत हो, अपितु ऐसा ईश्वरवाद होता है जो ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् के रूप में, एकमात्र आदि पुरुष के रूप में देखता है जो सभी कुछ को – चाहे जो कुछ भी हो, अच्छा-बुरा, सुख-दुःख, प्रकाश- अन्धकार - स्वयं अपनी ही सत्ता के पदार्थ के रूप में अपने अन्दर व्यक्त करते हैं और जो कुछ उन्होंने अपने-आप में व्यक्त किया है उसका स्वयं हो शासन करते हैं। द्वन्द्वों या अंतर्विरोधों से अप्रभावित, अपनी सृष्टि से अबद्ध इस प्रकृति से अतीत और फिर भी उसके साथ अंतरंग रूप से संबद्ध और उसके प्राणियों के साथ घनिष्ठ रूप से एकीभूत, वे, उनके आत्मा, अंतरात्मा परमात्मा, परमेश्वर, प्रेमी, सुहद्, आश्रय उन्हें उनके अन्दर से और ऊपर से अज्ञान और दुःख, पाप और प्रमाद के इन मर्त्य दृश्यों के भीतर ले जा रहे हैं, हर एक को उसकी प्रकृति के और सभी को विश्व-प्रकृति के द्वारा किसी परम् ज्योति, आनन्द, अमृतत्त्व और परात्परता की ओर ले जा रहे हैं।
यही मुक्तिप्रद ज्ञान की परिपूर्णता है। यह ज्ञान है उन भगवान् का जो हमारे अन्दर हैं और जगत् के अन्दर हैं और साथ ही विश्वातीत अनन्त हैं। वे परम निरपेक्ष जो अपनी दिव्य प्रकृति से, आत्ममाया से यह सब कुछ हुए हैं, वे अपनी विश्वातीत स्थिति में रहते हुए सबका शासन करते हैं। वे प्रत्येक प्राणी के अन्दर अंतरंग रूप से अवस्थित हैं और समस्त विश्व-घटनाओं के कारण, नियंता और चालक हैं और फिर भी इतने महान्, शक्तिशाली और अनन्त हैं कि अपनी सृष्टि से किसी प्रकार सीमित नहीं हो सकते। ज्ञान का यह स्वरूप भगवान् की प्रतिज्ञा के तीन पृथक् पृथक् श्लोकों में दिया गया है।
श्रीअरविन्द ने बड़े ही विस्तार से भगवान् के सारे ही भावों का वर्णन कर दिया है। इस सब में एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिये वह यह है कि वैसे ही जैसे कि अंतरिक्ष में अनंत आकाशगंगाएँ हैं और यदि हम अपनी अँगुलियों के इशारे से उन्हें बाँटना चाहें तो इससे उन आकाशगंगाओं के विराट् रूप पर कोई असर नहीं पड़ सकता, वैसे ही भले ही अपने मन के माध्यम से हम परमात्मा को किन्हीं भी सूत्रों में बाँधना या परिभाषित करना चाहें तो उससे परमात्मा के सत्स्वरूप पर कोई असर नहीं हो सकता। अतः हमें सदा ही इस चीज का भान होना चाहिये कि हमारे ऊँचे से ऊँचे मानसिक सूत्र भी परमात्मा के सत्स्वरूप का लेशमात्र भी निरूपण नहीं कर सकते। अतः अधिक से अधिक हम मन को व्यवहार के लिए और भगवान् की अभिव्यक्ति के लिए एक उपयोगी माध्यम के रूप में तो मान सकते हैं परंतु इससे अधिक हमें यह भ्रम करने की भूल नहीं करनी चाहिये कि उसके माध्यम से हम सत्य की अथवा भगवान् के स्वरूप की थाह पा सकते हैं। हालाँकि स्वयं व्यक्ति के लिए मन-बुद्धि के माध्यम से समझने का प्रयास करना व्यक्तिगत रूप से कुछ उपयोगी हो सकता है और संभवतः प्रयास करने से मन-बुद्धि में कुछ रूढ़िवादिता कम होकर उसमें सुनम्यता आ सकती है। परंतु इसके अतिरिक्त इसकी अधिक कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि हमारी किन्हीं भी मानसिक चीजों से भगवान् बंध नहीं जाते। यह तो वैसे ही है जैसे कि किसी अथाह सागर को लोटे में भर कर यह सोचना कि हमने सागर को उस लोटे में बाँध लिया है। जबकि वास्तव में परमात्मा तो इस उदाहरण से भी अचिंत्य रूप से अनंतआयामी और निरपेक्ष सत्ता हैं। उनके स्वरूप को तो कोई जान ही क्या सकता है। यदि इस बात को समझ लिया जाए तो इस कट्टरपंथी दृष्टिकोण पर कुछ अंकुश लग जाता है कि व्यक्ति का अपना ही मत या सत्य के विषय में केवल उसी का अनुभव एकमात्र स और अन्य सभी मत या दर्शन मिथ्या हैं। और साथ ही इस अहंकार दृष्टिकोण से पैदा होने वाली विषमता और वैमनस्य की चीजों पर भी भार अंकुश लग जाता है। यदि बुद्धि में यह सामान्य ज्ञान हो कि सभी दर्शन किसी बढई के उन अनेकों औजारों के समान हैं जिनकी यथासमय अिपनी-अपनी उपयोगिता है और सभी अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, तो उस बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है जिन्हें हम प्रायः ही इस सामान्य ज्ञान के अभाव में होते देखते हैं। इस नमनीयता के बिना तो व्यक्ति अपनी एक मानसिक कैद में बँधा होता है। और जब इस मानसिकता के साथ ही साथ व्यक्ति को यदि कोई आंशिक अनुभव प्रास हो जाता है तब तो वह अपने दृष्टिकोण के प्रति और अधिक सुनिश्चित हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप हम इतिहास में कितने ही अत्याचार घटित हुए देखते हैं। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि यहाँ ऋषियों-मुनियों, द्रष्टाओं, मनीषियों आदि की एक अटूट श्रृंखला रही है और सभी ने अपने-अपने तरीके से परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किया है। इस कारण यह एक आम समझ थी कि कोई भी निरूपण भगवान् के ही स्वरूप का कोई पक्ष उजागर कर रहा है परंतु कोई भी एक निरूपण या सभी निरूपण मिलाकर भी उनके सत्स्वरूप को पूर्ण रूप से उजागर नहीं कर सकते। इसीलिए एक प्रचलित प्रार्थना में हम कहते हैं कि यदि स्वयं सरस्वती भी अनंत काल तक भगवान् के गुणों को लिखती रहें, तो भी उनके गुणों का कोई पार या अंत नहीं आ सकता।
परंतु इस सब चर्चा का यह तात्पर्य नहीं निकाल लेना चाहिये कि मन की कोई उपयोगिता नहीं है। अवश्य ही हमारे निम्नतर भागों पर अंकुश लगाने में और जीवन के अंदर चीजों के बीच व्यवस्था स्थापित करने में उसकी उपयोगिता है। परंतु जैसा कि हम चर्चा कर ही आए हैं कि ज्ञान के उपकरण के रूप में मन को काम में लेना त्रुटि है। इसलिए महत्त्वपूर्ण बात है मन की सच्ची उपयोगिता समझ कर उसके अनुकूल उसे काम में लिया जाए। पशु के स्तर तक हम मानसिकता का विकास नहीं देखते। पशु अपनी सहज-वृत्ति (instinct) के द्वारा कार्य करता है और जब तक उसकी उस वृत्ति के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता तब तक वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो उसे संकट में डाल दे। इसी लिए हम पशु को सहज ही कोई जहरीली चीज खाते या कोई उसकी प्रकृति के प्रतिकूल व्यवहार करते नहीं देखते। परंतु मनुष्यों के साथ संपर्क के कारण हमारी मानसिकता द्वारा उसकी सहज-वृत्ति में हम कुछ हस्तक्षेप होता पाते हैं जिसके कारण पशु भ्रमित होकर बहुत बार विषाक्त चीजें खा लेते हैं, मनुष्य के बनाए जाल में फँस जाते हैं, अपनी सहज प्रवृति से हटकर क्रिया करने लगते हैं। पशुओं में आत्म-अवलोकन की शक्ति नहीं होती। केवल मानसिक चेतना ही है जिसमें आत्म- अवलोकन की शक्ति होती है जो अपने आप की क्रिया का अवलोकन और आकलन कर सकती है। यही आत्म-अवलोकन की शक्ति मनुष्य को पाशविकता से ऊपर उठा देती है और उसे सचेतन रूप से आगे गति करने की संभावना प्रदान करती है। इसी के द्वारा व्यक्ति अपनी निम्न वृत्तियों का अवलोकन कर सकता है, उनकी अराजक क्रीड़ा के ऊपर कुछ अंकुश लगा सकता है, जीवन में एक व्यवस्था लागू कर सकता है। और इसी के कारण सामूहिक जीवन सुचारू रूप से काम कर सकता है अन्यथा यदि बुद्धि न हो तो कभी किसी प्रकार के समाज की व्यवस्था नहीं की जा सकती। यदि समाज में नैतिक विधान न हों तो घोर अराजकता का साम्राज्य हो सकता है। मन और बुद्धि की यही उपयोगिता है। परंतु जब हम इसके इस सीमित दायरे से अधिक उस जगह इसे प्रयुक्त करने का प्रयास करते हैं जो इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है तब हम भयंकर भूल कर बैठते हैं। अतः जब गीता हमें परम वचन बताने जा रही है तो उसका पूरा लाभ उठाने के लिए यदि हम इन सभी बातों को ध्यान में रख कर एक उचित परिप्रेक्ष्य में उसकी शिक्षा को लें तो उससे यथासंभव लाभ उठा सकते हैं।
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।। ६।।
६. सात पुरातन महर्षि और चार मनु मेरे मानसिक आविर्भाव हैं; उनसे ही संसार में ये सब जीव उत्पन्न हुए हैं।
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ।। ७।।
७. जो कोई मनुष्य मेरे इस सर्वव्यापी ईश्वरभाव (विभूति भाव) को और पैरे इस योग को तात्त्विक रूप से जानता है, वह अविचल योग के द्वारा अपने-आप को मेरे साथ युक्त कर देता है, इस विषय में कोई संशय नहीं है।
..................
* महर्षि, जो वेदों की तरह यहाँ भी सात आदि-ऋषि, 'महर्षयः सप्त पूर्वे', जगत् के सप्त पुरातन कहे गये हैं, उस दिव्य प्रज्ञा की धी-शक्तियाँ हैं जिसने अपनी ही स्वात्म-सचेतन अनन्तता, 'प्रज्ञा पुराणी', से सब पदार्थों का विकास कराया है - अपने ही सार-तत्त्व के सात तत्त्वों की श्रेणियों को विकसित किया है।.... इनके साथ ही चार शाश्वत मनु, अर्थात् मनुष्य के जनक, हैं - क्योंकि परमेश्वर की क्रियाशील प्रकृति चतुर्विध है और मानवजाति इस प्रकृति को अपने चतुर्विध चारित्रिक लक्षण से प्रकट करती है। ये भी, जैसा कि उनके नाम से प्रकट होता है, मनोमय पुरुष हैं। इस समस्त जीवन के, जो अपनी क्रिया के लिए व्यक्त या अव्यक्त मानस पर निर्भर करता है, ये स्रष्टा हैं, उन्हीं से जगत् के ये सब प्राणणे उत्पन्न हुए हैं; सब उन्हीं की प्रजा और संतति हैं - येषां लोक इमाः प्रजाः। और ये महर्षि तथा ये मनु स्वयं भी परम् पुरुष के चिरंतन मानस पुत्र हैं जो उनकी आध्यात्मिक सर्वातीतला से विश्व-प्रकृति के अन्दर उत्पन्न हुए हैं- ये सब उत्पत्तिकर्ता हैं, परंतु जो कुछ भी विश्व में उत्पन्न होता है उस सबके मूलस्रोत तो परम् पुरुष ही हैं।
यहाँ किन्हीं मानवीय ऋषियों की नहीं अपितु 'धी' शक्तियों की बात हो रही है। इन महर्षियों की संख्या सात है। गीता में हम इसका विस्तृत वर्णन नहीं पाते परंतु वेदों में एन बारंबार यह सात की संख्या पाते हैं जिसमें चेतना के सात विभिन्न स्तर हैं - भौतिक प्राणिक, मानसिक, अतिमानसिक, सत्, चित् आऔर के सात विभिन हम अपने मन के द्वारा ही इन सात लोकों का अनुभव करते हैं। जड़तत्व का अनुभव भी हम अपने मन के द्वारा ही करते हैं। अन्य सभी लोकों का अनुभव भी हम उसी के माध्यम से करते हैं। साथ की महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और अनुभव भी हम उसी के माध्यम से कारोबार प्रका की प्रकृति पाते हैं। इससे संसार में उत्पन्न सभी जीवों का एक मोटा प्रारूप मिलता है।
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।। ८।।
८. मैं सभी कुछ की उत्पत्ति हूं और मुझसे ही सब कुछ कर्म और गतिरुप विकास में प्रवृत्त होता है; ऐसा जानकर ज्ञानी मनुष्य भावविभोर होकर मेरी भक्ति करते हैं।
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
कथयन्तश्व मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ।। ९॥
९. उनकी चेतना मुझसे परिपूर्ण होती है, उनका जीवन पूर्ण रूप से मुझे समर्पित होता है, परस्पर मेरा बोध करते हुए और मेरे विषय में चर्चा करते हुए, वे सदा ही संतुष्ट और हर्षित रहते हैं।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।। १०।।
१०. इन्हें, जो इस प्रकार मेरे साथ सतत् युक्त हैं और प्रेमजन्य तीव्र आनन्द से मुझे भजते हैं, मैं उस बुद्धियोग को देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त होते हैं।
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।। ११।।
१९. उनके ऊपर अनुकम्पा के कारण ही, मैं, उनकी आत्मा में स्थित हुआ, ज्ञान के प्रज्ज्वलित दीपक के द्वारा अज्ञानजनित अंधकार को नष्ट कर देता हूँ।
ये परिणाम अवश्यंभावी रूप से ज्ञान के स्वभावमात्र के कारण और उस योग के स्वभावमात्र के कारण उत्पन्न होते हैं जो उस ज्ञान को आध्यात्मिक संवर्द्धन और आध्यात्मिक अनुभव में परिणत कर देता है। क्योंकि मनुष्य के मन और कर्म की सारी परेशानी, उसके मन की, उसकी इच्छाशक्ति की, उसकी नैतिक प्रवृत्ति की, उसकी भावात्मक, संवेदनात्मक और प्राणिक उत्तेजनाओं की सभी लड़खड़ाहट, शंकाशीलता और वेदना या व्यथा का मूल उसके सम्मोह में अर्थात् उसके देह-बद्ध इन्द्रियाच्छादित मानव मन के लिए स्वाभाविक अंधकार में टटोलने की क्रिया और संज्ञान करने और निर्णय करने की भ्रांत क्रिया में मिल सकता है। परंतु जब वह सब पदार्थों के दिव्य मूल को देखता है, जब वह स्थिरभाव से विश्वदृश्य या प्रतीति से उसके विश्वातीत सत्स्वरूप को देखता है और फिर उस सत्स्वरूप से इस दृश्य को देखता है तब वह मन, बुद्धि, हृदय और इन्द्रियों के इस सम्मोह से मुक्त हो जाता है, असंमूढः मर्येषु, इस मृत्युलोक में प्रबुद्ध और मुक्त होकर विचरण करता है। हर चीज को अब केवल उसका वर्तमान और प्रतीयमान या बाह्य मूल्य प्रदान करने की बजाय उसे उसका परम और यथार्थ मूल्य प्रदान करते हुए वह इनके पीछे की गुप्त कड़ियों और संबंधों को ढूँढ़ लेता है; वह सारे जीवन और कर्म को सचेतन रूप से उनके उच्च और सच्चे उद्देश्य की ओर लगाता है और उन्हें उस प्रकाश और शक्ति के द्वारा संचालित करता है जो उसे उसके अंतःस्थ भगवान् से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह बोध करने या संज्ञान करने के गलत तरीके से, गलत मानसिक और ऐच्छिक प्रतिक्रिया से, इन्द्रियों के गलत रूप से ग्रहण करने से और उत्तेजना से, जो कि यहाँ पाप, प्रमाद और दुःख उत्पन्न करते हैं, छूट जाता है, सर्वपापैः प्रमुच्यते। क्योंकि इस प्रकार विश्वातीत और विश्वमय में निवास करते हुए वह अपने-आप को और दूसरे हर व्यष्टिरूप को उनके महत्तर रूपों अथवा मूल्यों में देखता है और अपनी पृथक्कारी और अहंकारमय बुद्धि व ज्ञान से उत्पन्न मिथ्यात्व और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक मुक्ति का सदा यही सारमर्म होता है ।
भगवान् यहाँ कह रहे हैं कि जो उनके साथ सतत् युक्त हैं और प्रेमजन्य तीव्र आनन्द से उन्हें भजते हैं, उन्हें वे बुद्धियोग प्रदान करते है प्रेमज उनकी आत्मा में स्थित होकर ज्ञान के प्रज्वलित दीपक के द्वारा और उजनित अंधकार को नष्ट कर देते हैं। इसकी व्याख्या करते हो श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि जिन परिणामों की श्रीकृष्ण चर्चा कर रहे हैं। अवश्यंभावी रूप से ज्ञान के स्वभावमात्र के कारण और उस योग के स्वभावमात्र के कारण उत्पन्न होते हैं जो उस ज्ञान को आध्यात्मिक संवर्द्धन और आध्यात्मिक अनुभव में परिणत कर देता है। सारे दिन ही हम देखते हैं कि किस प्रकार किसी छोटी सी घटना से, किसी प्रिय-अप्रिय संवेदन से, किसी प्रकार की सुखद या दुःखद प्राणिक उत्तेजना के कारण हम विचलित हो उठते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि अभी केवल हमारी देहगत चेतना से बंधी होती है और इंद्रियों आदि के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर ही चीजों का संज्ञान करती है और निर्णय करती है। साथ ही हमारे अंदर भिन्न-भिन्न भागों की क्रिया होती रहती है और जिस समय जो भाग सक्रिय होता है उसी के अनुसार हम व्यवहार करने लगते हैं। यदि नैतिक प्रकृति सक्रिय हो तो हम नैतिकता के अनुसार चीजों को देखने लगते हैं, भावनात्मक प्रकृति प्रधान हो तो हम चीजों को उस अनुसार देखने लगते हैं। भले ही हमारे सभी भागों के पास पूरे सत्य का कुछ-कुछ अंश तो है परंतु किसी के पास भी पूर्ण सत्य नहीं होता और किसी भी भाग का सत्य के ऊपर कोई एकाधिकार नहीं होता। इसलिए इन सभी भागों की भ्रांत क्रिया के कारण ही हमारा सारा कर्म भ्रांत और अज्ञानमव ही रहता है और हम सदा ही इस दुविधा में रहते हैं कि वास्तव में करें क्या। इन्हीं विभिन्न भागों की भिन्न-भिन्न आवाजों के कारण ही अर्जुन इस विषय में विचलित था कि आखिर उसे करना क्या चाहिये। इसी प्रश्न को लेकर गीता का आरंभ हुआ था। अर्जुन इसी दुविधा में था कि वह अपने गुरुजनों की हत्या कर ही कैसे सकता है। और यदि युद्ध न करे तो फिर अधर्म की विजय होगी और अधर्मी लोग निरंकुश अत्याचार करेंगे। तो फिर आखिर इस दुविधा का उपाय क्या है? इसका उपाय है वह ज्ञान जो सब पदार्थों के दिव्य मूल को देखता है, चीजों की गोचर प्रतीति से पो उसके विश्वातीत स्वरूप को देखता है और उसके अनुसार फिर इस दृत्ता जगत् को देखता है वह मन, बुद्धि, हृदय और इन्द्रियों के इस सम्मोह से मुक्त होकर प्रबुद्ध और मुक्त होकर विचरण करता है। जब तक व्यक्ति अतिशय रूप से अपने आप के ऊपर ही केंद्रित रहता है तब तक वह पूरे परिदृश्य को समझने में असमर्थ होता है इसलिए उसकी क्रिया भ्रांत होती है। ज्ञान के प्रभाव से व्यक्ति कुछ अधिक वैश्विक रूप से देख सकता है जिसके कारण उसे इस प्रतीति का मूल दिखाई देता है अतः वह चीजों के सच्चे स्वरूप को जान जाता है और उसी के अनुसार कर्म करता है। इसके कारण हमारे सभी भिन्न-भिन्न भागों के झूठे दावों की निरंकुश क्रिया पर रोक लग जाती है और इन सब भागों में अपना-अपना जो सत्य है उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। अतः उस ज्ञान के प्रकाश में इन सभी भागों की भ्रांत क्रिया की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। तब व्यक्ति प्रत्येक चीज के सत्य को जानकर उसे उसका उचित मूल्य प्रदान करता है और तब वह उन सब चीजों के पीछे की गुप्त कड़ियों को ढूँढ़ निकालता है कि किस प्रकार अपने मूल में वे चीजें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जब एक बार वह चीजों के मूल स्वरूप को जान जाता है तब वह अपने जीवन और कर्म को भगवान् से मिलने वाले प्रकाश और उनसे मिलने वाली शक्ति की सहायता से सचेतन रूप से उनके सच्चे उद्देश्य की ओर लगाता है। तब फिर और अधिक उसके मन आदि का कोलाहल और भ्रांतियाँ नहीं रहतीं। इसलिए वह बाहरी रूप से प्रतीत होने वाले कठोर से कठोर काम को भी सहजता से कर सकता है क्योंकि उसे तो भगवद्-प्रदत्त शक्ति प्राप्त होती है जिसके सामने उसे कोई चीज कठोर नहीं लगती। वास्तव में सामान्य मनुष्य को कठोरता तो इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि उसमें उन समस्याओं का सामना करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती। और यह सब कुछ उस योग के परिणामस्वरूप होता है जो 'उस ज्ञान को आध्यात्मिक संवर्द्धन और आध्यात्मिक अनुभव में परिणत कर देता है।' और तब व्यक्ति 'बोध करने या संज्ञान करने के गलत तरीके से, गलत मानसिक और ऐच्छिक प्रतिक्रिया से, इन्द्रियों के गलत रूप से ग्रहण करने से और उत्तेजना से, जो कि यहाँ पाप, प्रमाद और दुःख उत्पन्न करते हैं, छूट जाता है'। वास्तव में सत्ता के किसी भी भाग को उसके उचित महत्त्व से अधिक महत्त्व देना ही पाप है क्योंकि तब वह समग्रता के साथ समस्वर नहीं रहता। जब सभी चीजें आंतरिक सत्य के साथ समस्वरता में हों वही तो आदर्श स्थिति है। और उस ज्ञान और योग के प्रभाव से व्यक्ति विश्वातीत और विश्वमय में निवास करते हुए प्रत्येक व्यष्टिरूप को उसके महत्तर रूप और मूल्य के अनुसार देखता है और पृथक्कारी और अहंकारमय बुद्धि व ज्ञान से उत्पन्न मिध्यात्व और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। गीता के ये श्लोक इस बात का आश्वासन हैं कि यह योग इन परिणामों की ओर ले जाता है जिसमें व्यक्ति भगवान् के तीनों ही भावों को जान जाता है। भगवान् की इस समग्र दृष्टि के बाद ही व्यक्ति सभी चीजों को समग्रता में और समस्वरता में देख सकता है। अन्यथा केवल विश्वातीत स्वरूप को देखने पर वह इस जगत् अभिव्यक्ति को माया घोषित कर देता है, या केवल जगत् में व्याप्त परमात्मा को ही देखे तो इसमें लिप्त हो जाता है या फिर यदि केवल व्यष्टि को ही देखे तो भी संपूर्ण दृष्टि नहीं प्राप्त होती। इस विश्वमय स्वरूप को ही गलत रूप से लेने पर हम अनेक बार ऐसा सुनते हैं कि सभी जीव परमात्मा ही हैं अतः उनकी सेवा करनी चाहिये। मूलतः सत्य होने पर भी इस सत्य को हम इसके बाहरी अर्थ में लेकर भूल कर बैठते हैं। परंतु जब भगवान् के तीनों ही भावों का समग्र रूप से सच्चा बोध होता है तब व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म में कंपायमान नहीं होता, इसी को भगवान् कहते हैं 'अविकम्पेन योगेन', और यह सच्चा बोध तब होता है जब हृदय को भगवान् में आनंद आने लगता है।
अतः गीता की दृष्टि में, मुक्त पुरुष का ज्ञान कोई अमूर्त सम्बन्धरहित निर्व्यक्तिक की चेतना नहीं होता, कोई निष्क्रिय शांति या मौन नहीं होता। क्योंकि मुक्त पुरुष की मन-बुद्धि और हृदय दृढ़ रूप से सतत् इस बोध में और इस पूर्ण भाव में स्थित रहते हैं कि दिव्य जगत्पति की परिचालक और निर्देशनकारी सर्वव्यापी उपस्थिति (विभूति) द्वारा जगत् व्याप्त है, एतां विभूतिं मम यो वेत्ति। वह जानता है कि इस विश्व-व्यवस्था से उसकी आत्मा परे है, परंतु वह यह भी जानता है कि दिव्य योग से, योगं च मम, वह उसके साथ एक है। और वह इन विश्वातीत, विश्वगत और व्यष्टिगत सत्ताओं के हर पहलु को परम सत्य के साथ उसके यथोचित संबंध से देखता और सबको दिव्य योग के एकत्व में उनके यथास्थान में रखता है। वह अब और अधिक हर चीज को उसकी पृथक्ता में नहीं देखता - वह पार्थक्य दृष्टि जो अनुभव करने वाली चेतना के लिए या तो सभी परस्पर-सम्बन्धों को अस्पष्ट ही छोड़ देती है या केवल एक-पक्षीय रूप से प्रकट करती है। न वह सब चीजों को एक साथ गड्ड-मड्डू रूप में ही देखता है, - यह देखने का ऐसा अस्तव्यस्त तरीका है जो गलत ज्ञान और अव्यवस्थित कर्म देता है। विश्वातीत स्थिति में सुदृढ़ हुआ वह वैश्विक क्लेश से तथा काल और परिस्थिति की उथल-पुथल से प्रभावित नहीं होता। पदार्थों की इस सब सृष्टि और संहार के बीच में उसकी आत्मा विश्व में शाश्वत और आध्यात्मिक तत्त्व के साथ एक अचल, अकंपित और स्थिर योग में युक्त बनी रहती है।... वह भगवान् के स्वभाव और उनके धर्म के सदृश बन जाता है, साधर्म्यम् आगताः, जो विश्वभाव से भावित होने पर भी विश्वातीत और मन-प्राण-शरीर के विशिष्ट व्यष्टिरूप में रहकर भी वैश्वभावयुक्त होता है। यह योग जब एक बार सिद्ध हो जाता है तब ऐसे अविचल सुस्थिर योग के द्वारा, 'अविकम्पेन योगेन युज्यते', वह प्रकृति के किसी भी भाव को अपना सकता है, किसी भी मानव अवस्था को धारण कर सकता है, चाहे जो जगत्कर्म कर सकता है, बिना दिव्य आत्मस्वरूप के साथ अपने एकत्वभाव से च्युत हुए, परमेश्वर के साथ अपने निरन्तर मिलन से किसी भी हानि के बिना।
x7, xiv.2,x.8, xiii9
इस ज्ञान को जब अनुरागात्मक, भावपूर्ण और स्वभावगत स्तर में बदल दिया जाता है तब यह शांत स्थिर प्रेम और प्रगाढ़ भक्ति बन जाता है उन आदिकारण परात्पर ईश्वर के प्रति जो हमारे ऊपर हैं, जो यहाँ सब पदार्थों के स्वामी के रूप में सदा-विद्यमान हैं, मनुष्य में स्थित ईश्वर हैं, प्रकृति में स्थित ईश्वर हैं। यह ज्ञान सर्वप्रथम बुद्धि का ज्ञान होता है; परंतु इसके साथ-ही-साथ आती है भावमय प्रकृति की प्रेरित आध्यात्मिक अवस्था, बुधा भाव समन्विताः। हृदय और बुद्धि का यह परिवर्तन समस्त प्रकृति के सम्पूर्ण परिवर्तन का आरम्भ है। एक नया अंतर्जन्म और एक नया भूतभाव हमें हमारे प्रेम और भक्ति के परमाराध्य के साथ एकत्वलाभ के लिए, मद्भावाय, तैयार करता है। इस दिव्य परम सत्ता की, जो अब संसार में सर्वत्र और संसार के ऊपर भी दिखाई देती है, महत्ता, सौन्दर्य तथा पूर्णता में, प्रीति, प्रगाढ़ प्रेमानन्द प्राप्त होता है। वह प्रगाढ़ आनन्द, जो जीवन में छितरा हुआ और बाहरी सुख लेता है, उस मन का स्थान ग्रहण कर लेता है; या अधिक उचित रूप में कहें तो, वह आनन्द अन्य सभी सुखों को अपने अन्दर खींच लेता है और एक विलक्षण रसक्रिया के द्वारा मन और हृदय की सब भावनाओं और इन्द्रियों की सब क्रियाओं को रूपांतरित कर डालता है। संपूर्ण चेतना ईश्वर से परिपूर्ण हो जाती है और प्रत्युत्तर में आती उनकी चेतना से भर जाती है; संपूर्ण जीवन आनन्दानुभूति के अखण्ड समुद्र में प्रवाहित होने लगता है। ऐसे ईश्वर-प्रेमियों का समस्त संभाषण और चिंतन भगवान् के ही सम्बन्ध में परस्पर कथन और बोधन होते हैं। उस एक आनन्द में सत्ता का सारा संतोष और प्रकृति की सारी क्रीड़ा और सुख केन्द्रीभूत है। चिंतन और स्मरण में क्षण-प्रतिक्षण का सतर ऐक्य बना रहता है, आत्मा में ऐक्य की अनुभूति की अटूट निरंतरता बनी रहती है। और जिस क्षण से इस आंतरिक स्थिति का आरम्भ होता है उसी क्षण से, अपूर्णता की उस अवस्था में भी, भगवान् पूर्ण बुद्धियोग के द्वारा उसे दृढ़ करते हैं। वे हमारे अन्दर स्थित प्रज्वलित ज्ञानदीप को ऊपर उठाते हैं, पृथक्कारी मन और बुद्धि के अज्ञान को नष्ट कर देते हैं और मानव आत्मा के अन्दर स्वयं प्रकट होते हैं। इस प्रकार कर्म और ज्ञान के ज्ञानोद्दीप्त संयोजन पर आश्रित बुद्धियोग के द्वारा हमारे निम्नतर व्यथित मन की श्रेणियों से क्रियाशील प्रकृति के ऊपर स्थित साक्षी पुरुष की अक्षर शांति तक पहले ही संक्रमण सिद्ध किया गया था। परंतु अब एक सर्वसमावेशी ज्ञान के साथ एक प्रेम और भक्ति के ज्ञानोद्दीप्त ऐक्य के ऊपर आधारित इस महत्तर बुद्धियोग के द्वारा जीव एक बृहत् आनन्द के अंदर उन परम और सर्वप्रवर्तक ईश्वर के संपूर्ण परात्पर सत्य में ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार सनातन पुरुष व्यष्टिपुरुष और व्यष्टिप्रकृति में चरितार्थ हो जाते हैं; व्यष्टिपुरुष काल के अन्दर आवागमन से निकलकर सनातन की अनन्तताओं में प्रवेश कर जाता है।
-----------------------
* एक उच्च और शून्य निषेध ही सब कुछ नहीं है,
एक विशाल सर्वविलयन ही केवल 'परमेश्वर' का अंतिम वचन नहीं है,
जीवन का परम आशय, सत्ता के पथ का अंत नहीं है,
इस महान् रहस्यमय जगत् का यही अर्थ नहीं है।
चरम शांति में एक चरम 'शक्ति' सुप्त है।
जाग्रत होकर, यह समाधिबद्ध आत्मा को जागृत कर सकती है,
और किरण के अंदर उसके जनक-सूर्य को प्रकाशित कर सकती है:
इस जगत् को 'आत्मा' की शक्ति का आधार बना सकती है,
मिट्टी को लेकर 'परमेश्वर' का हूबहू रूप गढ़ सकती है।
और केवल एक सुप्त अंतरात्मा को मुक्त करना, तो ध्येय की ओर केवल एक ज्योतित पग है
जग में स्वयं को चरितार्थ करना ही 'प्रभु' की अभिलाषा थी।
II. भगवान् की संभूतिशक्ति
एक बड़ी महत्त्वपूर्ण अवस्था प्राप्त की जा चुकी है, गीता के आध्यात्मिक मुक्ति और दिव्य कर्मों के सिद्धांत के प्रतिपादनक्रम में तात्त्विक और मनोवैज्ञानिक समन्वय का एक निर्णायक निर्देश और जोड़ा जा चुका है। अर्जुन की बुद्धि में भगवान् प्रकट किये जा चुके हैं; बुद्धि की जिज्ञासा और हृदय की दृष्टि के समक्ष वे उन परमात्मा और जगदात्मा के रूप में, उन परम् पुरुष और विश्व-पुरुष के रूप में, हमारी सत्ता के उन अंतर्वासी भगवान् के रूप मैं प्रत्यक्ष कर दिये गये हैं जिन्हें मनुष्य का ज्ञान, संकल्प और भक्ति अज्ञान के धुँधले प्रकाश में ढूँढ़ रहे थे। इस प्राकट्य के अनेक पक्षों में से एक और पक्ष को पूर्ण करने के लिए अब केवल अनेकत्वपूर्ण विराट् पुरुष का दर्शन ही शेष है।
तात्त्विक समन्वय पूर्ण हो चुका। निम्न प्रकृति से जीव को पृथक् करने के लिये इसमें सांख्य को ग्रहण किया गया है - यह वह पृथक्करण है जो विवेकी बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान लाभ कर तथा प्रकृति के तीन गुणों के प्रति हमारी अधीनता को अतिक्रम कर के ही करना होता है। यह पृथक्करण संपूर्ण हो गया है और सांख्य की सीमाओं को पर-पुरुष और परा-प्रकृति के एकत्व का विशाल प्राकट्य कराकर अतिक्रम कर दिया गया है। अहंकार के चारों ओर बने हुए प्राकृत पृथक् व्यक्तित्व के आत्म-विलोपन के लिए दार्शनिकों का वेदान्त स्वीकृत किया गया है। क्षुद्र व्यष्टिसत्ता की जगह विशाल निर्व्यक्तिक सत्ता को स्थापित करने के लिए, पृथक्ता की भ्रांति को ब्रह्म के एकत्व की अनुभूति से मिटा देने और अहंकार की अंध दृष्टि के स्थान पर सब पदार्थों को एकमेव आत्मा के अंदर और एकमेव आत्मा को सब पदार्थों के अंदर देखने की सत्यतर दृष्टि ले आने के लिए वेदांत की पद्धति का प्रयोग किया गया है। वेदांत की इस पद्धति को उन परब्रह्म का समग्र दर्शन कराकर संपूर्ण कर दिया गया है जिनसे ही समस्त चर-अचर, क्षर-अक्षर, प्रवृत्ति-निवृत्ति की उत्पत्ति होती है। इसकी संभावित सीमाओं को उन परम् पुरुष परमेश्वर के अंतरंग दर्शन या प्राकट्य के द्वारा अतिक्रम कर दिया गया है जो समस्त प्रकृति में सब कुछ स्वयं बनते हैं, सब व्यष्टि जीवों के रूपों में स्वयं अपने-आप को प्रकट करते हैं और समस्त कर्मों में निज-प्रकृति की शक्ति प्रयुक्त करते हैं। मन, बुद्धि, हृदय और समस्त अंतःकरण का प्रकृति के प्रभु परमेश्वर के प्रति आत्म-समर्पण करने के लिए योग को ग्रहण किया गया है। इसकी संपूर्णता जगत् और जीवन के उन परम प्रभु को, जिनकी यह प्रकृतिस्थ जीव अंश सत्ता है, आदि-देव बनाकर साधित की गयी है। और, एक पूर्ण आत्मिक ऐक्य के प्रकाश में जीव का यह देख पाना कि सब पदार्थ प्रभु ही हैं, इससे योग को संभावित सीमाओं का अतिक्रमण किया गया है।
फलस्वरूप उन परम सत्स्वरूप भगवान् के, एक साथ ही, परात्पर सत्-तत्त्व, विश्व के विश्वातीत मूल के रूप में, सब पदार्थों के निर्व्यक्तिक आत्मा, विश्व के अचल धारक के रूप में, और सब प्राणियों, सब व्यष्टियों, सब पदार्थों, शक्तियों और गुणों के अंतःस्थित ईश्वर के रूप में, उस अंतर्यामी के रूप में जो सब भूतों के अंतर्बाह्य भाव, उनकी आत्मा और कार्यकारी प्रकृति हैं, - एक साथ ही इन सब रूपों में पूर्ण दर्शन होते हैं। उस 'एकमेव' के इस पूर्ण दर्शन और ज्ञान में ज्ञानयोग की उत्तम रूप से सिद्धि हो गयी। सब को का उनके स्वामी के प्रति समर्पण होने में कर्मयोग की पराकाष्ठा हो गयी,- क्योंकि प्राकृत मनुष्य अब भगवदिच्छा का केवल एक यंत्र रह जाता है। प्रेम और भक्ति का योग अपने विस्तृततम रूपों में बता दिया गया है। ज्ञान, कर्म और प्रेम की गहन पराकाष्ठा अंततः जीव और जीवेश्वर या परमात्मा के एक उच्चतम कोटि के ऐक्य को साधित करती है। उस ऐक्य में ज्ञान के रहस्योद्घाटनों को हृदय के लिए तथा बुद्धि के लिए यथार्थ बना दिया जाता है। उस ऐक्य में निमित्त मात्र होकर किये जानेवाले कर्म में कठिन आत्मोत्सर्ग सजीव एकत्व की सहज, मुक्त और आनंदमयी अभिव्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक मोक्ष का संपूर्ण साधन बता दिया गया है; दिव्य कर्म का संपूर्ण आधार निर्मित कर दिया गया है।
अर्जुन इस संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण करता है जो इस प्रकार दिव्य गुरु द्वारा उसे दिया गया है। उसका मन अपने संशयों और प्रयासों से मुक्त हो चुका है उसका हृदय, जो जगत् के बाह्य पक्ष से और उसकी चकित कर देने वाली बाह्य प्रतीति से हटकर अब अपने परम अर्थ और मूल तथा उसकी आंतरिक वास्तविकताओं की ओर मुड़ चुका है, शोक-संताप से छूटकर दिव्य प्रकटीकरण के अनिर्वचनीय आनंद के सम्पर्क में आ चुका है। इस ज्ञान को ग्रहण करने में जिस भाषा का उससे प्रयोग कराया जाता है वह ऐसी है कि उससे एक बार पुनः इस ज्ञान की गंभीर सर्वांगीणता और इसकी सर्वसमावेशी निर्णायकता और परिपूर्णता पर आग्रह और बल दिया गया है।
अब यहाँ हमें अर्जुन के मनोभाव में एक मूलभूत अंतर देखने को मिलता है। गीता अर्जुन के विषादयोग से आंरभ होती है जहाँ वह युद्ध करने के और उससे विरत होने के परिणामों के बीच दुविधा में था और यह चयन नहीं कर पा रहा था कि वह युद्ध करे या नहीं करे। इसलिए ऐसी मनोदशा से निकाल कर भगवान् उसकी बुद्धि को अनेकानेक विषयों पर अधिकाधिक आलोकित कर उसके अंदर भक्ति तत्त्व का संचार कर उसे अब इस सोपान तक ले आए हैं जहाँ उसके पूर्व के सभी विचलन अब नहीं रहे हैं और उसके हृदय को भगवान् में आनन्द अनुभव होता जा रहा है। उसे भगवान् में रस आने लगा है और भगवान् का परम वचन सुनकर उसके भाव पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं जो कि अगले ही श्लोकों की भाषा से स्पष्ट हो जाता है। अतः वही अर्जुन जो कुछ समय पूर्व अपने मर्म तक विचलित हो चुका था, उसी को अब हम आनंदित हो भगवान् का स्तवन करते देखते हैं।
अर्जुन उवाच
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ।। १२ ।।
१२. अर्जुन ने कहाः आप परंब्रह्म, परम् धाम, परम् पवित्र, एकमात्र शाश्वत और दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा, सर्वव्यापी प्रभु हैं।
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ।। १३।।
१३. समस्त ऋषि आपके विषय में ऐसा कहते हैं और नारद, असित, देवल, व्यास आदि देवर्षि भी ऐसा ही कहते हैं; और आप स्वयं भी मुझे ऐसा ही कहते हैं।
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ।। १४।।
१४. हे केशव! ये जो कुछ भी आप कहते हो उसे मेरा मन सत्य मानता है। हे भगवन्! आपके आविर्भाव को न देवता जानते हैं और न दानव।
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ।। १५।।
१५. हे समस्त भूतों को उत्पन्न करनेवाले, समस्त भूतों के ईश्वर, समस्त देवों के परमदेव, जगत् के प्रभो, हे पुरुषोत्तम! केवल आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने-आप को जानते हो।
अर्जुन सर्वप्रथम उन अवतार को, मानवस्वरूप में ईश्वर को, जो उससे बोल रहे हैं, उन्हें वह 'परं ब्रह्म, परं धाम' के रूप में मानता है जिनके अंदर जीव, इस बाह्य जगत् और इस अंशरूप भूतभाव से निकलकर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होने पर, रह सकता है। अर्जुन उन्हें 'पवित्रम् परमं', नित्य-मुक्त परम सत्ता की परम् पवित्रता के रूप में स्वीकार करता है जिस को व्यक्ति आत्मा की स्थिर-अचल और शांत अक्षर निर्व्यक्तिक ब्राह्मी स्थिति में अहं को मिटा देने पर प्राप्त करता है। इसके बाद वह उन्हें 'पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, एकमेव शाश्वत, सनातन दिव्य पुरुष के रूप में स्वीकार करता है। वह उन्हें 'आदि देव' कहकर उनकी स्तुति करता है और 'आदिदेवमजं विभुम्', उन अजन्मा की पूजा करता है जो सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी और संपूर्ण जगत् के आत्म-विस्तरणशील स्वामी हैं। इसलिए, वह उन्हें केवल उन 'अद्भुत' के रूप में ही नहीं मानता, जो किसी भी प्रकार के वर्णन से परे हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु उन्हें व्यक्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है, - "हे भगवान्, आपकी अभिव्यक्ति को न तो देवता जानते हैं न ही दानव", न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः - अपितु वह उन्हें सर्वभूतों के स्वामी, उनकी समस्त संभूति के एकमात्र दिव्य निमित्त कारण, देवों के देव, जिनसे सब देवता उद्भूत हुए हैं, तथा जगत् के पति के रूप में भी मानता है जो ऊपर से अपनी परा प्रकृति तथा विश्व-प्रकृति की शक्ति के द्वारा उसे अभिव्यक्त तथा परिचालित करते हैं, 'भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अंत में वह उन्हें हमारे अंदर तथा चारों ओर अवस्थित उन वासुदेव के रूप में ग्रहण करता है जो यहाँ सभी कुछ हैं अपनी संभूति की विश्वव्यापी, घट-घट वासी, सर्व-निर्मायक विभु-शक्तियों के बल पर, 'विभूतयः'...
उसने अपने हृदय की भक्ति, अपनी इच्छा-शक्ति के समर्पण तथा अपनी बुद्धि की समझ के साथ इस सत्य को ग्रहण कर लिया है। वह इस ज्ञान से युक्त होकर और इस आत्म-समर्पण के साथ दिव्य यंत्र के रूप में कार्य करने के लिए पहले ही तैयार हो चुका है। परंतु एक गंभीरतर सतत् आध्यात्मिक उपलब्धि की इच्छा अब उसके हृदय तथा उसकी संकल्पशक्ति में जगा दी गई है। यह एक ऐसा सत्य है जो केवल परम् आत्मा को ही अपने निज आत्म-ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है, - क्योंकि अर्जुन कह उठता है, "हे पुरुषोत्तम, केवल आप हो अपने-आप को अपने-आप के द्वारा जानते हैं", आत्मना आत्मनं वेत्थ । यह एक ऐसा ज्ञान है जो आध्यात्मिक तादात्म्य द्वारा प्राप्त होता है और प्राकृत मनुष्य का हृदय, संकल्प-शक्ति तथा बुद्धि उसकी सहायता के बिना, अपनी ही चेष्टा के द्वारा इस तक नहीं पहुँच सकते। ये तो केवल उन अपूर्ण मानसिक प्रतिबिंबों को ही प्राप्त कर सकते हैं जो इसे प्रकाशित करने से कहीं अधिक छिपाते तथा विकृत ही करते हैं। यह एक ऐसा गुप्त ज्ञान है जो मनुष्य को उन ऋषियों से सुनना होगा जिन्होंने इस सत्य का साक्षात्कार किया है, इसकी वाणी का श्रवण किया है और अंतरात्मा तथा आत्मा में इसके साथ एकात्मता प्राप्त की है। "सभी ऋषि और नारद, असित, देवल, व्यास आदि देवर्षि आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं।" अथवा मनुष्य को इसे अपने अंदर से अंतः-प्रकटन एवं अंतःप्रेरणा के द्वारा उन अंतःस्थित देव से प्राप्त करना होगा जो हमारे अंदर ज्ञान के प्रज्ज्वलित दीप को ऊपर उठाते हैं, "और आप स्वयं भी मुझे यही बताते हैं", स्वयंचैव ब्रवीषि मे। एक बार यह सत्य प्रकट हो जाने पर इसे मन की स्वीकृति, संकल्प-शक्ति की सहमति तथा हृदय का आनंद और स्वीकृति, पूर्ण मानसिक श्रद्धा के इन तीनों तत्त्वों के द्वारा स्वीकार करना होता है। अर्जुन ने इसे इसी प्रकार अंगीकार किया है; "इस सब को, जो आपने कहा है, मेरा मन सत्य मानता है।" परन्तु फिर भी हमारी सत्ता की आत्मा तक में तथा बाह्य सत्ता के अत्यंत अंतरंग चैत्य केन्द्र में भी गंभीरतर अधिकृति या अधिकार की आवश्यकता बनी रहेगी, उस नित्य अनिर्वचनीय आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए आत्मा की माँग बनी रहेगी जिसकी कि मानसिक जिज्ञासा तो एक प्रारंभिक रूप या छायामात्र है और जिसके बिना सनातन के साथ पूर्ण मिलन नहीं हो सकता।
वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ।। १६ ।।
१६. आप मुझे अपने दिव्य आत्माविर्भावों, अपनी विभूतियों के बारे में अशेष रूप से बताइये, जिनके द्वारा आप समस्त जगतों में व्याप्त होकर स्थित हैं।
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।। १७।।
१७. हे योगिन्! सर्वत्र और सर्वदा आपका ही चिन्तन करता हुआ मैं किस प्रकार आपको जानूँगा, और हे भगवन्! किन-किन प्रमुख आविर्भूत रूपों में मुझे आपका चिन्तन करना चाहिए?
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।
भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ।। १८ ।।
१८. हे जनार्दन! अपने योग को और विभूति को विस्तारपूर्वक और अधिकाधिक कहिए, क्योंकि यह मेरे लिए अमृतसुधास्वरूप है, और मैं इसे कितना भी सुनूँ मेरी तृप्ति नहीं होती है। "
इस प्रकार, उस उपलब्धि या साक्षात्कार तक पहुँचने का मार्ग अर्जुन से अब बता दिया गया है। और, जहाँ तक महान् स्वतःप्रत्यक्ष या स्वतःमिट दिव्य तत्त्वों का संबंध है, ये मन को चक्कर में नहीं डालते; वह पत्र देवाधिदेव के विचार, अक्षर आत्मा के अनुभव, अंतर्यामी ईश्वर के प्रत्यक्ष को देवा देव-न विश्व-पुरुष के संस्पर्श के प्रति खुल सकता है। एक बार मन जब देवाधिदेव-विषयक विचार से आलोकित हो जाता है, मनुष्य शीघ्रता के साथ मार्ग का अनुसरण कर सकता है और सामान्य मानसिक बोधों को अतिक्रांत करने के लिए चाहे कोई भी प्रारंभिक कठिन प्रयत्न क्यों न करना पड़े, फिर भी अंत में वह इन मूल सत्यों का, जो हमारी सत्ता तथा समस्त सत्ता के पौडे अवस्थित हैं, स्वानुभव प्राप्त कर सकता है, 'आत्मना आत्मानम्'। वह इसे इस शीघ्रता के साथ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये, एक बार विचार में आ जाने पर, प्रत्यक्ष ही दिव्य सत्य होते हैं; हमारे मानसिक संस्कारों में ऐसी कोई चीज नहीं जो ईश्वर को इन उच्च रूपों में स्वीकार करने से हमें रोकती हो। परंतु कठिनाई तो जीवन के प्रतीयमान सत्यों में उसे देखने, प्रकृति के इस तथ्य में तथा जगद्-अभिव्यक्ति के इस प्रच्छन्नकारी दृश्य प्रपंच में उसे ढूँढ़ निकालने में पैदा होती है; क्योंकि यहाँ सब कुछ इस उत्कृष्ट एकीकारक विचार के विपरीत है। भगवान् को मनुष्य, जीव-जन्तु तथा जड़ पदार्थ के रूप में, उच्च और नीच, सौम्य और रौद्र तथा शुभ और अशुभ में देखने के लिए हम कैसे सहमत हो सकते हैं? जगत् के पदार्थों में व्याप्त ईश्वर से संबंध रखने वाले किसी विचार को स्वीकार करके यदि हम ज्ञान की आदर्श ज्योति, शक्ति को महानता, सौंदर्य की मोहक छटा, प्रेम की उदारता तथा आत्मा की विपुल विशालता में उसे देख भी लें, तो भी इनके उन विरोधी गुणों के द्वारा, जो सचमुच ही इन उच्च वस्तुओं के साथ चिपके रहते हैं तथा उन्हें आच्छन्न और धूमिल कर देते हैं, एकता के भंग होने की बात से हम कैसे बचेंगे? और, यदि मानव-मन तथा प्रकृति की सीमाओं के बावजूद हम देव-पुरुष में ईश्वर को देख सकें, तो भी हम उन लोगों में उन्हें कैसे देखेंगे जो उनका विरोध करते हैं तथा कर्म और प्रकृति में उन सब चीजों को ही प्रकट करते हैं जिन्हें हम अदिव्य समझते हैं? यदि नारायण ज्ञानी और संत में बिना कठिनाई के गोचर हो जाते हैं तो भी पापी, अपराधी, वेश्या तथा चांडाल में वे हमें सुगमता से कैसे दिखाई देंगे? सर्वत्र परम पवित्रता तथा एकता की खोज करता हुआ ज्ञानी विश्व-सत्ता के सभी विभेदों के प्रति "यह नहीं, यह नहीं", 'नेति-नेति की कठोर पुकार करता है। यद्यपि हम इस संसार में बहुत-सी वस्तुओं को ऐच्छिक या अनैच्छिक स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा जगत् में भगवान् को स्वीकार करते हैं, तथापि क्या अधिकतर वस्तुओं के सामने मन को "यह नहीं, यह नहीं" की उस पुकार में ही नहीं डटे रहना होगा? यहाँ निरंतर ही बुद्धि की स्वीकृति, संकल्पशक्ति की सहमति और हृदय की श्रद्धा दृग्विषय और बाह्य रूप पर ही सदा सहारा लिये हुए मानव-मन के लिए कठिन हो जाती हैं। एकत्व की प्राप्ति के कठिन प्रयास के लिए कम-से-कम कुछ प्रबल संकेतों, कुछ श्रृंखलाओं और सेतुओं, कुछ अवलंबों की आवश्यकता पड़ती ही है।
यहाँ श्रीअरविन्द विभूति योग के महत्त्व का निरूपण कर रहे हैं। यदि यह स्पष्टीकरण न होता तो व्यक्ति के अंदर सामान्यतया जो धारणा रहती है कि परम वचन देने के बाद और एक ऐसा योग देने के बाद जब व्यक्ति अविकंपित होकर योग में दृढ़-प्रतिष्ठ हो जाता है, अब विभूतियोग बताने का आखिर औचित्य ही क्या है और इस योग की आवश्यकता ही क्या है। जब हम श्रीअरविन्द के आलोक में इसके अंदर प्रवेश करते हैं तब हमें गीता की अत्यंत विशाल योजना का भी बोध होता है जिसमें कि जो अंश सतही दृष्टि से हमें अधिक गंभीर प्रतीत नहीं होते, वे भी बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक अर्थ धारण कर लेते हैं जो हमारे समक्ष कुछ ऐसे गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं जो अन्यथा संभव ही नहीं थे।
-----------------------------------
* यहाँ हम गीता में एक ऐसी चीज का संकेत पाते हैं जिसे स्वयं गीता भी स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं करती, परंतु जो उपनिषदों में बार-बार आती है और जिसे आगे चलकर वैष्णव तथा शाक्त धर्मों ने, दर्शन की महत्तर तीव्रता में विकसित किया था, और वह है जगत् में रहनेवाले भगवान् में मनुष्य को आनंद प्राप्त होने की संभावना, सार्वभौम आनंद, जगज्जननी को क्रीड़ा एवं ईश्वर की लीला का माधुर्य और सौंदर्य।
प्रश्न : विभूति योग में ऐसा आता है कि भगवान् शुभ नहीं अपितु अशुभ में भी अभिव्यक्त हो रहे हैं। देवताओं में ही नहीं अपितु दानवों, राक्षसों आदि में भी अभिव्यक्त हो रहे हैं। मनुष्यों के लिए भगवान् की प्रकाशमय या शुभ या सौम्य अभिव्यक्तियों को तो सहज ही स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होती, परन्तु इनके विपरीत रूपों में उन्हें स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। जैसे कि, सरदार भगत सिंह ने अपनी पुस्तक 'मैं नास्तिक क्यों हूँ' में अपने नास्तिक होने के जो कारण दिए हैं उनमें से एक कारण यह है कि यदि भगवान् होते तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर इतने अन्याय और अत्याचार कैसे हो सकते थे। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में भगवान् की सत्ता को स्वीकार करना बहुत मुश्किल नहीं होता?
उत्तर : स्वयं अर्जुन के सामने भी तो एक भीषण स्थिति आ खड़ी हुई थी कि यदि वह युद्ध करता है तब भी उसके परिणाम उतने ही घातक होंगे जितने कि तब जब वह युद्ध से विमुख हो जाता है। यही बात तो सावित्री की माता ने कही कि परमात्मा का यह कैसा विधान है कि जिससे सावित्री विवाह करना चाहती है उस व्यक्ति की तो एक वर्ष के बाद मृत्यु निश्चित है। और ऐसा पहले से जानते हुए भी वह उसी से विवाह के लिए अड़ी हुई है। परंतु अर्जुन की वर्तमान स्थिति बदल चुकी है क्योंकि उसका हृदय तो अब भगवान् के सत्स्वरूप में आनंद लेने लगा है इसलिए उसकी स्थिति की दूसरे किन्हीं सतही उदाहरणों से तुलना नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति ने अभी तक भगवान् के स्वरूप का आस्वादन नहीं किया वह तो अवश्य ही इसी असमंजस में फंसा रहेगा कि भगवान् हैं भी या नहीं। अर्जुन की स्थिति का तो श्रीअरविन्द वर्णन कर ही रहे हैं कि, “...उस उपलब्धि या साक्षात्कार तक पहुँचने का मार्ग अर्जुन को अब बता दिया गया है। और, जहाँ तक महान् स्वतःप्रत्यक्ष या स्वतःसिद्ध दिव्य तत्त्वों का संबंध है, ये मन को चक्कर में नहीं डालते; वह परम देवाधिदेव के विचार, अक्षर आत्मा के अनुभव, अंतर्यामी ईश्वर के प्रत्यक्ष बोध तथा चेतन विश्व-पुरुष के संस्पर्श के प्रति खुल सकता है। एक बार मन जब देवाधिदेव-विषयक विचार से आलोकित हो जाता है, मनुष्य शीघ्रता के साथ मार्ग का अनुसरण कर सकता है और सामान्य मानसिक बोधों को अतिक्रांत करने के लिए चाहे कोई भी प्रारंभिक कठिन प्रयत्न क्यों न करना पड़े, फिर भी अंत में वह इन मूल सत्यों का, जो हमारी सत्ता तथा समस्त सत्ता के पीछे अवस्थित हैं, स्वानुभव प्राप्त कर सकता है, 'आत्मना आत्मानम्'।"
अतः, एक बार जब व्यक्ति को भगवान् का संस्पर्श प्राप्त हो जाता है तब उसमें भगवान् की सत्ता के विषय में सभी संशय आदि नष्ट हो जाते हैं और तब वह पूरे संकल्प और मनोयोग के साथ, बिना भ्रमित हुए सीधे अपने गंतव्य की ओर गति कर सकता है अन्यथा तो यदि व्यक्ति को अभी भगवान् की सत्ता के विषय में कोई जीवंत अनुभव प्राप्त नहीं होता तो उसे अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई निर्णायक दिशा प्राप्त नहीं होती और उसके कर्म भ्रमित ही होते हैं। एक बार जीवंत अनुभव प्राप्त होने पर स्वतः ही जीवन में निर्णायकता या निश्चयात्मकता आ जाती है और व्यक्ति पूर्ण संकल्पशक्ति के साथ अपने मार्ग पर अग्रसर होता है। यही कारण है कि साक्षात्कार प्राप्त होने के पश्चात् साधक बिना किसी प्रकार के विचलन के एकनिष्ठ रूप से अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाता है। और तब फिर उसके निमित्त किसी प्रकार का भी कर्म, भले घोर से घोर कर्म भी क्यों न हो, व्यक्ति के लिए सहज हो जाता है और ऐसा कर के वह भगवान् की अधिकाधिक अंतरंगता प्राप्त कर सकता है।
परंतु वर्तमान पार्थिव अभिव्यक्ति के अंदर हम देखते हैं कि शुभ के साथ ही अशुभ, सुंदर के साथ ही वीभत्स आदि चीजें भी घुली-मिली रहती हैं तो ऐसे में सभी के अंदर समान ही रूप से भगवान् के दर्शन कैसे किये जाएँ। इसीलिए विभूति का महत्त्व है। उसकी सहायता से जहाँ कहीं भी भगवान् का विशेष प्राकट्य होता है व्यक्ति उसे अधिक सहजता से पहचान सकता है। और फिर विभूति योग के बाद तो भगवान् अपना विश्वरूप दर्शन ही प्रकट कर देते हैं जिसमें कि अर्जुन को सारा विश्व उन्हीं का विग्रह दिखाई देता है।
पार्थिव अभिव्यक्ति के विषय में हम एक भिन्न दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। सर्वत्र ही, और विशेषकर हमारी भारतीय संस्कृति में सदा ही 'असतो मा सद्गमय' जैसे सूत्रों पर बल दिया जाता रहा है। हमें सदा ही सिखाया जाता रहा है, और हमारे अंदर भी यह अंतर्निहित है कि हमें प्रकाश और अंधकार में से प्रकाश को ही चुनना चाहिये, सत्य और असत्य के बीच सत्य का ही वरण करना चाहिये क्योंकि मनुष्य के मन की जैसी बनावट है उसके अनुसार उसे इन द्वंद्वों के बीच चयन करना होता है। स्वयं श्रीमाँ भी कहती हैं कि, "जीवन सत्य और मिथ्यात्व के बीच, प्रकाश और अंधकार, प्रगति और अवनति, ऊँचाइयों की ओर आरोहण या रसातल में पतन के बीच निरंतर चुनाव है। हर एक को चयन की स्वतंत्रता है।" (CWM 14, 29)
ऐसा इसलिए है क्योंकि मन के विभाजक स्वभाव के कारण शुरू से ही हमारे अंदर चयन करने का अभ्यास होता है। और व्यक्ति को यदि सचेतन चयन का बोध न हो तो व्यावहारिक जीवन में बड़ी विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी क्योंकि वह तो किन्हीं भी चीजों के बीच चयन नहीं कर पाएगा। इसलिए चयन करना हमारी आवश्यकता है। परंतु इसके साथ ही हमें यह भान भी होना चाहिये कि यह चयन हम अपने मानदंडों के अनुसार करते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम सहज ही समझ सकते हैं। यदि कोई समझदार आदिमानवों का झुंड जगत् के अंदर भगवान् की क्रिया का आकलन करने लगे तो आखिर वह कितना सार्थक होगा? वहीं कोई चींटी यदि अपने दृष्टिकोण से यह आकलन करने लगे तब वह कैसा होगा? यदि कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी आदि भी यह आकलन करें तो कदाचित् वे यही कहेंगे कि भगवान् जैसी किसी चीज की कोई सत्ता हो ही नहीं सकती अन्यथा तो मनुष्य उनके ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार करते हैं वे तो संभव ही नहीं थे, और अत्याचार करने के बाद भी मनुष्य बड़े ऐशो-आराम से रहते हैं जबकि उनका जीवन सदा ही संकटमय बना रहता है। इसलिए इससे हमें यह समझना चाहिये कि चूंकि ये सभी दृष्टिकोण अपने एक सीमित अहं के अंदर बँधे होने के कारण एकांगी रूप से चीजों को देखते हैं इसलिए कोई भी मानदंड परमात्मा की क्रिया के ऊपर कभी भी लागू नहीं हो सकते। इसीलिए श्रीअरविन्द कहते हैं कि हमें अर्जुन की अपेक्षा कम व्यथित दृष्टि से काल और मृत्यु के हमारे स्वामी का दर्शन करना होगा और इस वैश्विक-संहारकर्ता को अस्वीकार करने, इससे घृणा करने या इससे भयभीत होने की वृत्ति को छोड़ देना होगा और परमात्मा को कल्याणकारी जननी के रूप में ही नहीं अपितु रक्तरंजित संहार-नृत्य करनेवाली, करालवदना काली के रूप में भी स्वीकार करना होगा और ऐसा देखकर व्यक्ति को इस श्रद्धा के आधार पर खड़ा होना होगा कि 'भले तुम मुझे मार भी डालो, फिर भी मैं तुम्हारा भरोसा ही करूंगा।' ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति को यह श्रद्धा रखनी होगी कि भले उसे देखने में जो कुछ भी प्रतीत होता हो फिर भी भगवान् की क्रिया उसके लिए सदा ही कल्याणकारी ही होती है। जैसे कि बच्चे को किसी शल्य क्रिया में भले कितनी भी पीड़ा क्यों न हो परंतु तो भी उसे यह विश्वास होता है कि उसकी माँ उसके हित के लिए ही सब कुछ करेगी। मनुष्य के साथ सामान्यतः यही समस्या होती है कि विषम परिस्थितियों में उसके लिए यह मनोभाव रखना मुश्किल होता है। लोग बाहरी घटनाओं के आधार पर, परिस्थितियों आदि के अनुसार, अनुकूलता-प्रतिकूलता के अपने मानसिक मानकों के अनुसार यह विचार करने लगते हैं कि आखिर भगवान् हैं भी या नहीं। परंतु कम से कम बुद्धि के स्तर पर ही हमें यह समझ होनी चाहिये कि इतनी विशाल सृष्टि हमारे किन्हीं मानसिक मानदंडों के अनुसार नहीं चल सकती। सभी के अपने-अपने पूर्वाग्रह और मानक होते हैं और परमात्मा को यदि इनका सम्मान करना होता या इनसे बाध्य होना पड़ता तब तो कभी कोई चीज हो ही नहीं सकती थी क्योंकि स्वयं किसी एक व्यक्ति में ही समय-समय पर परस्पर विरोधी भाव उठते रहते हैं। और यह भी एक सत्य है कि मनोवैज्ञानिक रूप से भगवान् के विषय में हम जैसी आशा करते हैं उसी रूप में वे हमें प्रत्युत्तर भी देते हैं। स्वयं गीता में चौथे अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में भगवान् कहते हैं कि, 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अर्थात् मनुष्य जिस किसी भी रूप से मेरे समीप आते हैं उन्हें मैं उस ही रूप में प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हूँ।' हालाँकि वर्तमान प्रसंग में अर्जुन की यह स्थिति नहीं है। वह तो भगवान् के स्वरूप में आनंद अनुभव करने लगा है और चाहता है कि किस प्रकार वह अधिकाधिक भगवान् की छवि को हर चीज में देख पाए। इसी के उत्तर में भगवान् कहते हैं कि चूंकि उनके विस्तार का कोई अन्त नहीं है इसलिए वे केवल अपनी प्रधान विभूतियों के विषय में ही बता सकते हैं।
यद्यपि अर्जुन 'सर्व' के रूप में वासुदेव के प्राकट्य को स्वीकार करता है और यद्यपि उसका हृदय इसके आनंद से परिपूर्ण है, - क्योंकि वह पहले से ही अनुभव कर रहा है कि यह उसे उसके मन की व्याकुलता से और उन स्खलनकारी विभेदों से मुक्त कर रहा है जिनके लिए उसका मन किसी सूत्र, या किसी संकेत के लिए पुकार कर रहा था, एक द्वंद्वमय या विरोधमय जगत् की चकराने वाली समस्याओं के बीच किसी मार्गनिर्देशक सत्य के लिए पुकार कर रहा था, और यह उसके कानों के लिए अमृत-सुधा, 'अमृतम्' है, - फिर भी वह ऐसे अवलंबों और संकेतों को प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि एक पूर्ण तथा सुदृढ़ उपलब्धि की कठिनाई को दूर करने के लिए ये अनिवार्य हैं; क्योंकि और किस प्रकार से इस ज्ञान को हृदय तथा जीवन की वस्तु बनाया जा सकता है? वह मार्गदर्शक संकेत चाहता है, यहाँ तक कि वह श्रीकृष्ण से अपनी संभूति की सर्वोच्च शक्तियों को पूर्ण रूप से तथा विस्तार के साथ गिनाने के लिये प्रार्थना करता है और चाहता है कि उसकी दृष्टि से कुछ भी छूटने न पाये, उसे चकरा देने के लिए कोई भी चीज शेष न रहे।
श्रीभगवान् उवाच
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।। १९।।
१९. श्रीभगवान् ने कहाः हे कुरुश्रेष्ठ! हाँ, अब मैं तुझे अपनी दिव्य विभूतियों के विषय में बताऊँगा, किंतु केवल प्रधान विभूतियों के बारे में ही कहूँगा, क्योंकि विश्व में मेरे आत्मविस्तार के विवरणों का कोई अन्त नहीं है।
दिव्य गुरु शिष्य की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु शुरू में स्मरण करा देते हैं कि पूर्ण उत्तर देना संभव नहीं है। क्योंकि ईश्वर अनंत है और उनकी अभिव्यक्ति भी अनंत है। उनकी अभिव्यक्ति के रूप भी असंच हैं। प्रत्येक रूप अपने अंदर छिपी हुई किसी दिव्य शक्ति, 'विभूति' का प्रतीक है और किसी समर्थ दृष्टि के लिए प्रत्येक 'सीमित' अनंत के विशिष्ट प्राकट्य को अपने अंदर वहन करता है। वे कहते हैं, 'हाँ' मैं तुम्हें अपनी दिय विभूतियों के बारे में बताऊँगा; परंतु केवल अपनी कुछ प्रमुख विभूतियों के विषय में तथा निर्देश के रूप में और उन वस्तुओं के उदाहरण के द्वारा जिनमें तुम देवाधिदेव की शक्ति को अत्यंत सहजता से देख सकते हो, प्राधान्यक्तः, उद्देशतः। क्योंकि, जगत् में ईश्वर के आत्म-विस्तार के असंख्य विवरणों का कोई अंत नहीं है, नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। इस बात को स्मरण कराकर हो गुरु इस प्रकरण का आरंभ करते हैं और इसे और अधिक तथा असंदिग्ध बल देने के लिए अंत में इसे पुनः दुहराया गया है। और फिर शेष सारे अध्याय में हम जगत् के पदार्थों तथा प्राणियों में विद्यमान दिव्य शक्ति के इन प्रमुख निर्देशों, इन उत्कृष्ट लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन पाते हैं। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है मानो ये बिना किसी क्रम के ही अस्तव्यस्त रूप में दे दिये गये हों, परंतु फिर भी इनके परिगणन में एक विशेष नियम-क्रम है जो, यदि एक बार हमारे सामने प्रकट हो जाए तो, हमें एक सहायक पथ-प्रदर्शन के द्वारा इस विचार तथा इसके परिणामों के आंतरिक आशय की ओर ले जा सकता है।
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एव च ।। २० ।।
२०. हे गुडाकेश (निद्रा-विजयी) अर्जुन! मैं आत्मा हूँ जो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। मैं समस्त भूतों का आरम्भ और मध्य और अन्त भी हूँ।
आदित्यानामहं विष्णुर्थ्योतिषां रविरंशुमान् ।
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्रणामहं शशी ।। २१।।
२१. आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों और दीप्तियों में मैं देदीप्यमान सूर्य हूँ; मरुतों में मैं मरीचि हूँ: नक्षत्रों में मैं चन्द्रमा हूँ।
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
इन्द्रियाणां मनश्वास्मि भूतानामस्मि चेतना ।। २२॥
२२. वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं वासव (इन्द्र) हूँ, और इन्द्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों में मैं चेतना हूँ।
रुद्राणां शंकरश्वास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
वसूनां पावकश्वास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ।। २३ ।।
२३. रुद्रों में मैं शिव हूँ, यक्ष और राक्षसों में धनपति कुबेर हूँ और वसुओं में अग्नि हूँ, पर्वत-शिखरों में मैं मेरु हूँ।
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ।। २४।।
२४. हे पार्थ! मुझे पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति जान; और मैं सेनानायकों में (युद्ध का देवता) स्कन्द हूँ, सरोवरों में मैं सागर हूँ।
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ।। २५।।
२५. महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में मैं एकाक्षर ॐ हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ, स्थावरों (पर्वत श्रृंखलाओं) में मैं हिमालय हूँ।
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ।। २६॥
२६. पेड़-पौधों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, और देवर्षियों में नारद हूँ, गन्धवर्षों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ।
उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ।। २७।।
२७. मुझे अश्वों में अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक अश्व जान; श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत जान, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ।
आयुधानामहं वजं धेनूनामस्मि कामधुक् ।
प्रजनश्वास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८॥
२८. अत्रों में मैं दिव्य वज्र हूँ, गायों में कामधेनु (श्री-समृद्धि देने वाली गाय) हूँ और प्रजनकों (सन्तानोत्पादकों) में काम-देव हूँ, सपर्षों में वासुकि हूँ।
अनन्तश्वास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ।। २९।।
२९. नागों में मैं अनन्त (शेषनाग) हूँ, और समुद्री जीवों में वरुण है, और दिव्य पितरों में अर्यमा हूँ, नियम और विधान की रक्षा करनेवालों में मैं पर (नियम का देवता) हूँ।
प्रह्लादश्वास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्व पक्षिणाम् ।। ३० ।।
३०. दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूँ, जो गणना (आकलन) और माप करते हैं उनमें काल हूँ; और जंगली पशुओं में मैं उनका राजा सिंह हूँ और पक्षियों में क्ष वैनतेय (गरुड़) हूँ।
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
झषाणां मकरश्वास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ।। ३१।।
३१. निर्मल करने वालों में मैं वायु हूँ, शत्रधारी योद्धाओं में मैं राम हूँ, मत्स्यों में मकर हूँ, और नदियों में मैं गंगा नदी हूँ।
सर्गाणामादिरन्तश्व मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ।। ३२॥
३२. हे अर्जुन! मैं सृष्टि की उत्पत्ति और मध्य और अन्त भी हूँ। ज्ञान की अनेक शाखाओं में मैं आध्यात्मिक ज्ञान हूँ, विवाद करनेवालों का मैं तर्क हूँ।
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ।। ३३॥
३३. अक्षरों में मैं 'अ' हूँ और समासों में द्वन्द्व समास हूँ, मैं ही अविनाशी काल हूँ, मैं समस्त सृष्टि का धारण करनेवाला हूँ जिसके मुख सब ओर हैं।
मृत्युः सर्वहरश्वाहमुद्भवश्व भविष्यताम् ।
कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ।। ३४॥
३४. और मैं सर्व-भक्षी मृत्यु हूँ, और जो भविष्य में उत्पन्न होनेवाले हैं उनका उद्भव भी मैं ही हूँ। स्त्रीलिंगी गुणों में मैं कीर्ति, सौंदर्य, वाणी, स्मृति, धी (बुद्धि), दृढ़ता और क्षमा हूँ।
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ।। ३५।।
३५. मैं साम मंत्रों में बृहत्साम भी हूँ, छन्दों में गायत्री हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं बसन्त हूँ।
द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ।। ३६ ।।
३६. छल करनेवालों में मैं जुआ हूँ; तेजस्वियों का मैं तेज हूँ, मैं दृढ़ निश्चय और विजय हूँ: सात्त्विक मनुष्यों (सत्पुरुषों) का मैं सत्त्वगुण हूँ।
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ।। ३७।।
३७. मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव कृष्ण हूँ: पाण्डवों में अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यास और कवियों में उशना (शुक्राचार्य) कवि हूँ।
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ।। ३८॥
३८. शासनकर्ताओं का मैं राजदण्ड हूँ, जो सफल होने और जीतने की चेष्टा करते हैं उनकी मैं नीति हूँ; गुह्य पदार्थों में मैं मौन हूँ और ज्ञानवान् व्यक्तियों का मैं ज्ञान हूँ।
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ।। ३९।।
३९. और हे अर्जुन! समस्त भूतों का जो कुछ भी बीज है वह मैं ही हूँ; ऐसा कोई भी चर या अचर भूत नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्वमान रह सकता हो।
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ।। ४०।।
४०. हे परंतप! मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं, केवल (संकेतों या लक्षणों के तरीके से ही) मैंने मेरी विभूतियों के विस्तार को संक्षेप में कहा है।
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ।। ४१।।
४१. जो कुछ भी ऐश्वर्यशाली, सौन्दर्ययुक्त, अथवा बलशाली और शक्तिशाली है उस सभी को तू निश्चय ही मेरे तेज के एक अंश से उद्भूत हुआ जान।
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ।। ४२।।
४२. परंतु हे अर्जुन! इस सब विवरण को जानने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? (इसे इस प्रकार ही जान लो कि) इस संपूर्ण जगत् को मैं अपने अत्यंत क्षुद्र अंश से धारण किये हुए हूँ।
इतना कुछ बता कर भी भगवान् कहते हैं कि यह सब तो उनकी आभा का एक अतिशुद्र अंश है। कम से कम हमारी बुद्धि में इससे इतना प्रकाश तो आ ही जाना चाहिये कि भले ही व्यावहारिक तौर पर तो हमें जितनी बुद्धि प्राप्त है उसे प्रयोग में लेना आवश्यक है, परंतु हमारे कोई भी ऊँचे से ऊँचे मापदण्ड भी परमात्मा को बाँध नहीं सकते, उनकी थाह नहीं पा सकते। यदि यह भान हो तो फिर इस चीज की कुछ संभावना रहती है कि हम किसी प्रकार के अतिशय व्यवहार से बच सकते हैं जो कि एकांगी प्रकार की विचारधारा में देखने को मिलता है।
प्रश्न : यहाँ वेदों में ऋग्वेद की बजाय सामवेद को विशिष्ट क्यों बताया गया है?
उत्तर : सामवेद में मंत्र तो ऋग्वेद से ही हैं। सामवेद अपने आप में पृथक् नहीं है। उसे तो छन्द बद्ध किया गया है। बाकी, सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद ही है। परंतु साम गान के कारण सामवेद को यहाँ विशिष्टता प्रदान की गई है।
यदि हम गुण और मात्रा के विभेदों से या भिन्न-भिन्न मूल्यों तथा प्रकृति के द्वंद्वों या विरोधों से अंधे हुए बिना... चीजों का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि सभी वस्तुएँ वस्तुतः इस अभिव्यक्ति की शक्तियाँ हैं, इस विश्वव्यापी आत्मा तथा अध्यात्म-सत्ता की विभूतियाँ हैं, इस महान् योगी का योग, इस अद्भुत आत्मस्रष्टा की आत्म-सृष्टि हैं, और इसके सिवा वे और कुछ हो हो नहीं सकतीं ।... परन्तु अपनी संभूति में विद्यमान शक्ति के द्वारा ही दृष्टिगोचर होने के कारण वे हमें उस चीज में विशेष रूप से दिखायी देते हैं जो उत्कृट मूल्य-महत्त्व रखती है या जो प्रबल तथा श्रेष्ठ शक्ति के साथ कार्य करतो प्रतीत होती है। अतएव, सत्ता के प्रत्येक प्रकार या किस्म में हम उन्हें उनमें हो अधिक-से-अधिक देख सकते हैं जिनमें उस प्रकार या किस्म की प्रकृति को शक्ति सर्वोच्च, प्रमुख तथा अत्यंत प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्ति को प्राप्त करती है। वे एक विशेष अर्थ में उच्चतम शक्ति और अभिव्यक्ति भी अनंत का केवल एक अत्यंत आंशिक आत्म-प्रकटनकारी प्राकट्य ही होती है; यहाँ तक कि यह संपूर्ण ब्रह्माण्ड भी उनकी महिमा के एक अंशमात्र से अनुप्राणित हो रहा है, उनकी ज्योति की केवल एक किरणमात्र से प्रकाशित हो रहा है, उनके आनंद और सौंदर्य की एक हल्की-सी झलकमात्र से ही महिमान्वित हो रहा है। यही, संक्षेप में, इस परिगणन का सार तथा उससे निकलनेवाला परिणाम है और यही इसके अर्थ का मर्म है।
भगवान् अपनी सत्ता में इतने विशाल और इतने महान् हैं कि कोई विशिष्ट से विशिष्ट विभूति भी उनका केवल एक अतिक्षुद्र अंश ही प्रकट करती है। भगवान् का आनंद, उनकी शक्ति, उनका ज्ञान आदि सब उनकी सत्ता का, उनके सत्स्वरूप का एक छोटा सा अंश ही हैं। हम जितनी भी ऊँची से ऊँची कल्पना कर सकते हैं उससे और जो कभी कल्पना कर ही नहीं सकते उस सबसे भी भगवान् अनन्त रूप से परे हैं। और फिर भी जो कुछ भी इस पार्थिव अभिव्यक्ति में है वह सब वे स्वयं ही हैं। और इसके साथ ही साथ यह भी एक परम सत्य है कि भगवान् की सत्ता में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य की सत्ता में निहित न हो। संपूर्ण ब्रह्माण्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य में न हो। यही तो भगवान् की लीला है। मन के लिए तो भौतिक विश्व की थाह पाना ही संभव नहीं है। फिर इनसे ऊपर प्राणिक, मानसिक, अतिमानसिक आदि जगत् हैं। और ये सभी मनुष्य के अंदर निहित हैं। इसलिए भगवान् की जो बाह्य अभिव्यक्ति है उसके सहारे मनुष्य भगवान् के अधिकाधिक निकट पहुँच सकता है। इसी कारण विभूति और अवतार तत्त्व बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।
[इस अध्याय को 'विभूति-योग' का नाम दिया गया है], जो एक परमावश्यक योग है। क्योंकि, जहाँ हमें विश्वव्यापी दिव्य 'संभूति' के साथ उसके संपूर्ण विस्तार में, उसके शुभ और अशुभ, पूर्णता और अपूर्णता, प्रकाश और अंधकार में समभाव से अपने-आप को एकाकार करना होगा, वहाँ हमें साथ-ही-साथ यह भी अनुभव करना होगा कि इसके अंदर एक आरोहणशील विकासात्मक शक्ति है, वस्तुओं में इसके प्राकट्य की बढ़ती हुई गहनता है, कोई क्रम-परंपरात्मक रहस्यमय वस्तु है जो हमें प्रारंभिक आवरणकारी प्रतीतियों से, उत्तरोत्तर उच्चतर रूपों में से गुजारती हुई, विश्वव्यापी देवाधिदेव की व्यापक आदर्श प्रकृति की ओर ऊपर उठा ले जाती है।
यदि हम इस दृश्यमान बाह्य-तथ्य को ही देखते हैं कि हमारी अपनी प्रकृति है और दूसरों की प्रकृति है, तो हम अज्ञान की दृष्टि से देख रहे होते हैं और सब में, सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक प्राणी में, देव और दानव में, संत और पापी में, ज्ञानी और अज्ञानी में, बड़े और छोटे में, मनुष्य, पशु, वनस्पति तथा जड़ सत्ता में समान रूप से ईश्वर को नहीं जान सकते। एत दृष्टि तो प्राकृत सत्ता के संपूर्ण गुह्य सत्य के रूप में एक साथ तीन चीजों देखती है। प्रथमतः और प्रधानतः वह सब में दिव्य प्रकृति को निगूढ़, विद्यमान तथा विकास के लिए प्रतीक्षारत देखती है; वह उसे सब वस्तुओं में विश्वमार यथार्थ शक्ति के रूप में देखती है, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो विभिन्न मु और शक्ति के इस समस्त बाह्य क्रियाकलाप को उसका मूल्य प्रदान करती है और गुण एवं शक्ति-रूपी इन बाह्य विषयों का अर्थ वह इनकी अपनी अहं और अज्ञान की भाषा में नहीं करती अपितु दिव्य प्रकृति के प्रकाश में करने है। इसलिए, द्वितीयतः, वह देव और राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी और सरोमा (रेंगने वाले), सज्जन और दुर्जन, मूर्ख और विद्वान् में बाह्य क्रिया के भेदों को भी देखती है, पर इन अवस्थाओं में, इन छद्मरूपों की आड़ में होते हुए दिख गुण और शक्ति की क्रिया के रूप में देखती है। वह आवरण या मुखौटों के कारण बहकावे में नहीं आ जाती, अपितु प्रत्येक आवरण के पीछे परमेश्वर को खोज निकालती है। वह विकृति या अपूर्णता को देख लेती है, परंतु उसे बेघ कर उसके पीछे विद्यमान आत्मा के सत्य तक जा पहुँचती है, इतना ही नहीं, बल्कि वह उसे उस विकृति एवं अपूर्णता में भी ढूँढ़ निकालती है जो अपने-आप से अंधी बनी हुई है, अपने स्वरूप को पाने के लिए संघर्ष कर रही है। आत्म-अभिव्यक्ति और अनुभूति के अनेक रूपों के द्वारा अपनी आत्मा के पूर्ण ज्ञान, अपने अनंत और चरम रूप पर पहुँचने के लिए अंधवत् टटोल रहो है। मुक्त दृष्टि विकृति और अपूर्णता पर अनुचित बल नहीं देती, अपितु सबको, हृदय में पूर्ण प्रेम और उदारता, बुद्धि में पूर्ण समझ तथा आत्मा में पूर्ण समता रखते हुए, देखने में समर्थ होती है। अंततः, वह अपने-आप को संसिद्ध या अभिव्यक्त करने के लिए प्रयासरत शक्तियों की ईश्वर की ओर ऊर्ध्वमुखी तीव्र-प्रवृत्ति को देखती है; शक्ति और गुण की सभी उच्च अभिव्यक्तियों का देवत्व की जाज्वल्यमान जिह्वाओं का, निम्नतर प्रकृति के स्तरों से समुज्ज्वल प्रज्ञा और ज्ञान, महान् शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, साहस, वीरता, प्रेम और आत्म-दान के सौम्य माधुर्य, उत्साह और गौरव, उत्कृष्ट सद्गुण, श्रेष्ठ कर्म, मोहक सुषमा तथा समस्वरता, सुन्दर तथा दिव्य सृजन के शिखरों की ओर ऊपर उठी हुई अपनी प्रखरताओं से युक्त आत्मा, मन और प्राण की आरोही महानताओं की वह आदर, अभिनंदन और प्रोत्साहन करती है। आत्मा की दृष्टि महान् विभूति के अंदर मनुष्य के ऊपर उठते हुए देवत्व को देखती और उसे पहचान लेती है।
मुक्त दृष्टि साथ ही साथ तीन चीजों को देखती है। पहले, वह सभी के अंदर भगवान् की पराप्रकृति को निहित देखती है जो कि अपने आप को अधिकाधिक प्रकट करने की प्रतीक्षा में है। दूसरे, वह बाहरी आवरण से भ्रमित हुए बिना उसके पीछे भी दिव्य प्रकृति की क्रिया को कार्यरत देखती है। और तीसरे वह यह देखती है कि सभी कुछ के अंदर एक आरोही क्रम में भगवान् की विभूति अभिव्यक्त हो रही है। यों तो सभी में भगवान् की वर्धित होती अभिव्यक्ति का क्रम चल ही रहा है परंतु जब किसी चीज में भगवान् की विशेष अभिव्यक्ति प्रकाशित होती है तो उसे विभूति की संज्ञा देते हैं। और ये विभूतियाँ किसी काल या देश से मर्यादित नहीं हैं अपितु सदा ही प्रकट होती रहती हैं। और भगवान् की विशिष्ट अभिव्यक्ति मनुष्य तक भी सीमित नहीं है अपितु वह तो किसी भी चीज में हो सकती है। श्रीमाताजी कहती थीं कि किसी मकान को भी भगवान् को अभिव्यक्त करने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक मनुष्य को। केवल अपने अहं के कारण ही मनुष्य के लिए इस बात को सही रूप में ले पाना बहुत कठिन है।
उसका वह पहचानना परमेश्वर को शक्ति के रूप में पहचानना है, परंतु शक्ति यहाँ अपने व्यापकतम अर्थ में अभिप्रेत है, अर्थात् केवल बल के रूप में ही शक्ति अभिप्रेत नहीं है, अपितु ज्ञान, संकल्प, प्रेम, कर्म, पवित्रता, मधुरता तथा सुन्दरता की शक्ति के अर्थ में भी अभिप्रेत है। भगवान् सत्ता (सत्), चेतना (चित्) और आनंद हैं, और इस जगत् में सभी कुछ अपने-आप को बाहर प्रक्षिप्त करके व्यक्त करता है, और फिर सत्ता की शक्ति तथा चेतना एवं आनंद की शक्ति के द्वारा अपने-आप को पुनः प्राप्त कर लेता है; यह दिव्य शक्ति के कार्यों का जगत् है। वह शक्ति यहाँ अपने-आप को असंख्य प्रकार के भूतों में रूपान्वित करती है और उनमें से प्रत्येक भूत में उस दिव्य शक्ति की अपनी-अपनी निजी विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक शक्ति उस रूप के अंदर विद्यमान स्वयं भगवान् ही हैं... त्रिगुण के द्वारा उत्पन्न किया गया विकार वास्तव में मुख्य नहीं, अपितु गौण पहलू है; महत्त्वपूर्ण वस्तु तो वह दिव्य शक्ति है जिसे आत्म-अभिव्यक्ति मिल रही है। भगवान् ही स्वयं को महान् मनीषी, वीर, जननायक, महान् गुरु, ज्ञानी, पैगम्बर, धर्म-संस्थापक, संत, मानवप्रेमी, महाकवि, महान् कलाकार, महान् वैज्ञानिक, तप-परायण आत्म-वशी, वस्तुओं व घटनाओं तथा शक्तियों को वश में करनेवाले मनुष्य में प्रकट करते हैं। स्वयं वह कृति, वह उच्च काव्य, पूर्णांग सुंदर रूप, गहरा प्रेम, उदात्त कर्म, दिव्य उपलब्धि ईश्वर की हो क्रिया होती है; वह अभिव्यक्तिगत भगवान् ही होते हैं।
जितने भी गुण हैं, जितने भी उत्कृष्ट कर्म या भाव या कृतियाँ हैं वे सभी परमात्मा की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। जब भी हमें कहीं कोई विशिष्ट गुण प्रकट हुआ मिलता है तब हमें उसे परमात्मा की ही विशिष्ट अभिव्यक्ति के रूप में देखना चाहिये। समस्त महत्ता तो भगवान् की ही है, सभी कुछ उन्हीं की सत्ता से प्रकाशित है, उनके अतिरिक्त तो किसी का अपना पृथक् अस्तित्व और अपना पृथक् प्रकाश तो है ही नहीं। और सच्चा मनोभाव है जहाँ-कहीं और जिस-किसी रूप में भी भगवान् प्रकट होते हैं उसे देखकर आनंदित होना क्योंकि वास्तव में तो सभी चीजें हैं ही इसलिए कि उनमें भगवान् अभिव्यक्त हो सकें। केवल हमारा अहं या ईर्ष्या आदि अन्य चीजें ही हैं जो हमें दूसरों के अंदर भगवान् की विशिष्ट अभिव्यक्ति को देखने से रोकती हैं। यदि हम अपने अहं और पूर्वाग्रहों से बाहर आकर देख पाएँ तो हम पाएँगे कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान् की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है जो अन्य किसी में नहीं मिल सकती। जब हम इस दृष्टिकोण से देखने लगेंगे तो हमारे अंदर एक अद्भुत आश्चर्य का भाव होगा कि किस प्रकार भगवान् प्रत्येक के अंदर एक विशेष प्रकार की लीला कर रहे हैं। कहीं किसी के अंदर वे शौर्य अभिव्यक्त करते हैं, कहीं किसी के अंदर दया अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे ही वे किसी के अंदर दृढ़ता तो किसी के अंदर माधुर्य अभिव्यक्त करते हैं। यदि हम इस दृष्टिकोण से देख पाएँ तो हमारा संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा और हम सर्वत्र भगवान् की ही अभिव्यक्ति के दर्शन करके सदा ही आनंद में मग्न रहेंगे। परंतु वर्तमान में हम बाहरी मुखौटों से इतने अधिक भ्रमित रहते हैं कि उनके पीछे अभिव्यक्त होते उन परमात्मा को चूक जाते हैं और इस कारण उस अभिव्यक्ति में हमें जो आनन्द प्राप्त हो सकता था उससे भी चूक जाते हैं और हमारा जीवन दुःखमय बना रहता है। सारी प्रकृति के माध्यम से स्वयं परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। एक सच्चा कलाकार या एक कवि उसी तत्त्व को उजागर करने का प्रयास करता है जिससे हमारी आँखें प्रायः चूक जाती हैं। और जितना ही अधिक वह उस तत्त्व को उजागर करने में सफल रहता है उतना ही अधिक मूल्य उसकी कृति का होता है।
प्रश्न : जब गीता सातवें अध्याय के उन्नीसवें श्लोक में कहती है कि 'वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः' तब फिर क्या ये दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण नहीं हुए जहाँ एक के अंदर व्यक्ति सभी में परमात्मा के दर्शन करता है और जबकि दूसरे दृष्टिकोण में विभूति के रूप में उनकी विशिष्ट अभिव्यक्ति को देखकर उसके प्रति विशिष्टता का भाव रखता है?
उत्तर : इनमें कोई विरोधाभास या फिर अंतर नहीं है। व्यक्ति सभी के अंदर परमात्मा के दर्शन तो करता ही है परंतु साथ ही उसे यह बोध भी होता है कि परमात्मा की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर वर्धमान है। तत्त्वत्तः परमात्मा तो सभी के अंदर विद्यमान हैं ही परंतु उनकी अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न होती है। यह वैसे ही है जैसे कि वही अध्यापक भिन्न-भिन्न श्रेणी की कक्षाओं में उनके अनुसार ही अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। यदि इस वर्धित होती अभिव्यक्ति को न समझा और स्वीकार किया जाए तो बहुत सी गुत्थियाँ समझ में नहीं आ सकतीं। हम एक क्रमविकासमय जगत् में हैं जहाँ प्रकृति भगवान् के तत्त्व को प्रकट करने के लिए नए-नए रूपों 'का निर्माण करती है। परंतु असंख्यों ब्रह्माण्डों का निर्माण करने पर भी परमात्मा इन सब से छूट निकलते हैं। इसीलिए मुक्त दृष्टि को तीनों ही दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। वह देख लेती है कि सभी के अंदर परमात्मा व्याप्त हैं, और न केवल शुभ में अपितु अशुभ रूपों में भी वे ही विद्यमान हैं और साथ ही यह कि परमात्मा की उत्तरोत्तर बढ़ती अभिव्यक्ति हो रही है। इसीलिए श्रीअरविन्द कहते हैं कि श्रीकृष्ण के स्वरूप के विषय में जो कुछ भी आज तक प्रकट किया गया है वह सब भी उनके सत्स्वरूप का एक अतिक्षुद्र अंश ही है। उनका सत्स्वरूप तो इन सबसे अनंत रूप से परे है। इसलिए जिस रूप में मनुष्यों ने भगवान् श्रीकृष्ण के सौंदर्य का, उनके माधुर्य का चित्रण और वर्णन किया है वह अवश्य ही सत्य है, परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि उनका सौंदर्य और माधुर्य इन सब चित्रणों और वर्णनों से अनंनतः अधिक है जो कि अचिंत्य है और कल्पनातीत है। अवतारों के प्राकट्य में भी हम उनके विषय में भिन्न-भिन्न कलाओं का वर्णन पाते हैं। इससे हमें उनके आरोही प्राकट्य का ही दर्शन होता है अन्यथा तो भिन्न-भिन्न अवतारों का भिन्न-भिन्न कलाओं से संपन्न होने का वर्णन करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए विभूति तत्त्व जो है वह 'वासुदेवः सर्वमिति' कथन का परिपूरक ही है। और इसीलिए भगवान् के विशिष्ट प्राकट्य को, जहाँ कहीं उनकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से होती है उसे बहुत महत्त्व दिया जाता रहा है, उसकी पूजा की जाती रही है, उसे आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जहाँ कहीं और जिस किसी में भी किन्हीं विशिष्ट गुणों का प्राकट्य हुआ है उसे हमारी संस्कृति में सदा ही आदर्श माना गया है और उसकी कथाएँ अब भी हमें प्रेरित करती हैं।
इन सब विशिष्ट प्राकट्यों के बाद भी यह क्रमविकास इतना मुश्किल है कि यदि अवतारों के रूप में परमात्मा स्वयं हस्तक्षेप न करते तो इस विकासमय प्रक्रिया को सुचारू रख पाना प्रकृति के लिए संभव नहीं था। और जब तक कि अतिमानसिक अवतरण नहीं हो जाता तब तक अवतारों की आवश्यकता रहती है। क्योंकि, जैसा कि हम चौथे अध्याय में अवतार विषय में विशद चर्चा कर ही चुके हैं कि अवतार के आने से क्रमविकास को सहारा मिलता है। भगवान् जब अवतरित होकर आते हैं तब वे स्वयं विभूति भी होते हैं और अवतार भी होते हैं।
मानव जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आता है जब व्यक्ति का मन किसी भी प्रकार भगवान् के किसी रूप में, उनकी किसी छवि से इतना आकृष्ट हो जाए, उसमें इतना रम जाए कि उससे बाहर निकल पाना उसके लिए संभव ही न रहे। उसके प्रभाव से फिर समर्पण अधिक शीघ्रता से हो सकता है। क्योंकि एक बार जब मन भगवान् की छवि में रम जाता है तब उसके सहारे अहं से छुटकारा पाना अपेक्षाकृत अधिक आसान हो जाता है। यदि भगवान् के प्रति यह आकर्षण न हो तो केवल किन्हीं बाहरी साधना पद्धतियों आदि के माध्यम से अहं की ग्रंथि को सुलझा पाना सहज ही संभव नहीं है। व्यक्ति के अंदर यह आकर्षण अपने गुरु के लिए, किसी महापुरुष के लिए या अन्य किसी के लिए हो सकता है। परंतु एक सीमा से बाहर जाने पर आकर्षण जीवन में एक निर्णायक परिवर्तन ले आता है और व्यक्ति को अपने आप को भूलने में बहुत सहायता मिलती है। भागवत् पुराण में हम शिशुपाल की कथा सुनते हैं कि किस प्रकार अपने जन्मकाल से ही वह भगवान् से इतना द्वेष रखता था कि सोते-जागते हर समय उन्हीं के विषय में भला-बुरा सोचता और कहता था। इसलिए उसके वध के बाद जब उसकी परम सद्गति देखकर युधिष्ठिर ने आश्चर्यचकित हो नारद जी से प्रश्न किया कि ऐसी सद्गति तो कदाचित् ही किसी को प्राप्त हो, तो नारद जी ने कहा कि भले द्वेष भाव से ही सही परंतु भगवान् का सतत् चिंतन जैसा वह करता था वैसा तो कदाचित् ही कोई करता हो इसीलिए जो सद्गति उसे प्राप्त हुई है वह भी कदाचित् ही किसी के लिए संभव है। हालाँकि इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि द्वेष भाव से भगवान् का चिंतन किया जाए, इसकी बजाय श्रेष्ठ है प्रेम से उनका चिंतन करना। और जब व्यक्ति प्रेम से उनका चिंतन करता है, उनके प्रति आकृष्ट होता है तब अहं की गाँठें गलनी शुरू होती हैं। अन्यथा तो किसी भी प्रकार हमारा अहं हमें नहीं छोड़ता। पर एक बार जब हमें भगवान् की रूप माधुरी में आनंद आने लगे तो उनका कोई प्रसंग, उनके विषय में कोई चर्चा या अन्य कोई चीज भी हमें बिल्कुल विभोर कर सकती है। उस अवस्था में व्यक्ति को उनके अतिरिक्त और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सारे वैष्णव तंत्र का एकमात्र यही प्रयास है कि किसी भी प्रकार व्यक्ति का मन भगवान् में रम जाए। अतः, विभूति योग से हम यह अर्थ भी लगा सकते हैं कि जगह-जगह भगवान् के विशिष्ट प्राकट्य से हम उनकी ओर आकृष्ट होते हैं और उसके माध्यम से अपने आप को भूलने में हमें बहुत सहायता मिलती है।
यह एक ऐसा सत्य है जिसे सभी प्राचीन संस्कृतियाँ स्वीकार करती थीं और इसका आदर करती थीं, परंतु आधुनिक मन के एक पक्ष को इस विचार के प्रति एकदम घृणा है, वह इसमें निरे शक्ति-सामर्थ्य की पूजा, अज्ञानपूर्ण या आत्म-पतनकारी वीरपूजा या आसुरी अतिमानव के सिद्धांत को ही देखता है। निःसंदेह ही जैसे सभी सत्यों को ग्रहण करने का एक अज्ञानी तरीका है वैसे ही इस सत्य को ग्रहण करने का भी एक अज्ञानी तरीका है; परंतु प्रकृति की दिव्य व्यवस्था में इसका अपना एक विशेष स्थान, एक अनिवार्य कार्य है। गीता इसे उसी समुचित स्थान तथा परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने रखती है। इसे सभी मनुष्यों तथा सब प्राणियों में विद्यमान दिव्य आत्मा के अभिज्ञान पर आधारित होना होगा; इसे बड़ी और छोटी, प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध सभी अभिव्यक्तियों के प्रति एक समान हृदय से सुसंगत होना होगा। ईश्वर को अज्ञानी, दीन, दुर्बल, पापी तथा पतित, सभी में देखना और उनसे प्रेम करना होगा। स्वयं विभूति में भी, केवल भगवान् के एक बाह्य प्रतीक के रूप में तो भले ही, अन्यथा उसके बाह्य स्वरूप या व्यक्तित्व में उसे इस प्रकार स्वीकृत और उच्चासीन नहीं किया जाना है, अपितु उस एकमात्र देवत्व को स्वीकृत और उच्चासीन किया जाना है जो अपने-आप को उस शक्ति में प्रकट करता है। परंतु इससे यह तथ्य रद्द नहीं हो जाता कि अभिव्यक्ति में एक चढ़ती हुई श्रृंखला है और प्रकृति अपनी आत्म-अभिव्यक्ति के क्रमों में अपने अंधेरे में टटोलते हुए, अंधकारमय या अप्रकाशित प्रतीकों से परमेश्वर की प्रथम प्रत्यक्ष अभिव्यक्तियों की ओर ऊपर आरोहण करती है। प्रत्येक महान् सत्ता, प्रत्येक महान् उपलब्धि उसकी आत्म-अतिक्रमण की शक्ति का चिह्न है और साथ ही अंतिम और परम अतिक्रमण का आश्वासन है। स्वयं मनुष्य भी पशु तथा रंगनेवाले जीवों की अपेक्षा प्राकृतिक अभिव्यक्ति की एक उच्चतर श्रेणी है। यद्यपि दोनों में वही एक 'समं ब्रहा' विद्यमान है। परंतु मनुष्य अभी अपने अद्याप अतिक्रमण के उच्चतम शिखरों तक नहीं पहुँचा है और इस बीच उसके अंदर अपने-आप को चरितार्थ या अभिव्यक्त करने की महान् शक्ति की प्रत्येक झलक को एक आश्वासन और एक लक्षण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। महान् अग्रणियों के पद-चिह्नों की ओर दृष्टिपात करने से, जो उसे उपलब्धि के चाहे किसी भी सोपान से अतिमानवता की ओर ले जाते हैं या संकेत करते हैं, मनुष्य में, सभी मनुष्यों में अवस्थित दिव्यता के लिये हमारा आदर कम नहीं होता, अपितु बढ़ता ही है और साथ ही उसे एक अधिक परिपूर्णतर अर्थ भी प्राप्त होता है।....
विश्व की आत्मा के रूप में वह शक्ति सब के प्रति सम है, अतएव प्रत्येक मनुष्य को वह उसकी प्रकृति के व्यापारों के लिए जो आवश्यक है वह प्रदान करता है; किन्तु पुरुषोत्तम का मनुष्य के साथ वैयक्तिक सम्बन्ध भी है जिसमें वे उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से निकट हैं जो उनके पास पहुँच गया है। ये सब शूरवीर और महारथी, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहे युद्ध में सम्मिलित हुए हैं, भगवत्संकल्प के पात्र हैं और प्रत्येक के द्वारा वे उसकी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, पर उसके अहं के पर्दे की ओट में ही। अर्जुन उस बिंदु पर पहुँच गया है जहाँ आवरण को विदीर्ण किया जा सकता है तथा देहधारी भगवान् अपनी विभूति के सम्मुख अपनी कार्यशैली का रहस्य प्रकाशित कर सकते हैं। और सत्य का दर्शन कराया जाए, ऐसा आवश्यक भी है। वह एक महत् कार्य का निमित्त भी है, एक ऐसा कार्य जो देखने में तो भीषण है पर मानवजाति के प्रयाण में आगे की ओर एक लंबा कदम उठाने के लिए तथा धर्मराज्य, 'ऋतम्' और 'सत्यम्' के राज्य की स्थापना हेतु उस द्वारा किये जानेवाले संघर्ष में एक निर्णायक गति के लिए आवश्यक है। मानव के युग-चक्रों का इतिहास मानवता की अंतरात्मा और उसके जीवन में ईश्वर के अनावरण या उद्घाटन की ओर प्रगति है; उसकी प्रत्येक महान् घटना और अवस्था एक दिव्य अभिव्यक्ति है। गुप्त भागवत्-संकल्प के प्रधान यंत्र, महान् नायक, अर्जुन को वह दिव्य मानव बनना होगा जो उस महत् कार्य को सचेतन रूप से, भगवान् के कार्य के रूप में करने में समर्थ हो। इस प्रकार करने से ही वह कर्म आन्तरात्मिक रूप से सजीव बन सकता है तथा अपना आध्यात्मिक महत्त्व और अपने गुप्त अर्थ की ज्योति एवं शक्ति प्राप्त कर सकता है। उसे आत्मज्ञान के लिए आह्वान प्राप्त हुआ है; उसे ईश्वर को विश्व के स्वामी तथा जगत् के प्राणियों और घटनाओं के मूल के रूप में तथा सब को प्रकृति के अन्दर परमेश्वर की आत्म-अभिव्यक्ति के रूप में देखना होगा, तथा सब के अन्दर ईश्वर को देखना होगा, अपने अन्दर मानव तथा विभूति के रूप में ईश्वर को ही अनुभव करना होगा, सत्ता की निम्नताओं में तथा उसकी ऊँचाइयों पर, उच्च-से-उच्च शिखरों पर ईश्वर को ही देखना होगा, उसे मनुष्य को भी ऊँचाइयों पर विभूति के रूप में, तथा परम मोक्ष और मिलन में अंतिम शिखरों की ओर आरोहण करते हुए देखना होगा। उत्पत्ति और संहार के कर्म में अपने पग रखते हुए काल को भी उसे परमेश्वर की मूर्ति के रूप में देखना होगा, - ऐसे पग जो सृष्टि के उन विकास चक्रों को पूरा करते हैं जिनकी गति के आवर्तों पर मानव-देह में अवस्थित दिव्य आत्मा जगत् में ईश्वर की विभूति के रूप में उनका कार्य करता हुआ परमोच्च परात्परताओं की ओर ऊपर उठता है। यह ज्ञान प्रदान कर दिया गया है; भगवान् का काल-रूप अब प्रकट किया जाना है और उस रूप के कोटि-कोटि मुखों से मुक्त-विभूति के सम्मुख नियत कर्म के लिए आदेश निःसृत होनेवाला है।
विभूतियोग का यही निष्कर्ष है कि सभी जगह हम भगवान् की उत्तरोत्तर वर्धमान अभिव्यक्ति के दर्शन कर सकते हैं। और इसका सच्चा लाभ तो तब है जब भगवान् की कोई अभिव्यक्ति हमें इस सीमा तक अभिभूत कर दे कि फिर हमारा मन उसी में रम जाए और हमें उन्मत्त कर दे। अन्यथा तो अपने आप के विचार से, अपने अहं से, अपने गठन से मुक्त हो पाना संभव नहीं है।
इस प्रकार दसवाँ अध्याय 'विभूतियोग' समाप्त होता है।
ग्यारहवाँ अध्याय
I. विश्वरूपदर्शन संहारक काल
विश्व-पुरुष का दर्शन गीता के उन सुप्रसिद्ध प्रकरणों में से है जो अत्यंत ओजस्वी रूप में काव्यमय हैं, परन्तु गीता की विचारधारा में इसका स्थान सर्वथा सतह पर प्रकट नहीं है। और निःसंदेह ऐसा किसी काव्यात्मक तथा सत्योद्भासक प्रतीक के लिए अभिप्रेत भी होता है (कि वह अपना अभिप्राय सतह पर प्रकट नहीं करता) और इसके आशय को ग्रहण कर सकने के पूर्व हमें देखना होगा कि इसका सूत्रपात कैसे तथा किस प्रयोजन से किया गया है, साथ ही यह भी जानना होगा कि अपने अर्थगर्भित रूपों में यह किस बात की ओर संकेत करता है। अदृष्ट भगवान् की जीवंत मूर्ति तथा प्रत्यक्ष महिमा को, जगत् का संचालन करनेवाले परम् आत्मा और शक्ति के साक्षात् विग्रह को देखने की इच्छा से अर्जुन ने ही इसके लिए प्रार्थना की है।
अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।॥ १॥
१. अर्जुन ने कहाः मेरे ऊपर अनुग्रह कर के आपने जो सत्ता के उच्चतम आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करनेवाले वचन कहे; इससे मेरा मोह (भ्रम) दूर हो गया है।
[अर्जुन ने] सत्ता के इस सर्वोच्च आध्यात्मिक रहस्य का श्रवण कर लिया है कि सब कुछ भगवान् से उत्पन्न होता है तथा सब कुछ भगवान् है और सभी चीजों में भगवान् निवास करते तथा गुप्त रूप से विद्यमान हैं और प्रत्येक सीमित दृश्यवस्तु में उन्हें प्रकट किया जा सकता है। वह भ्रम जो मनुष्य के मन तथा इन्द्रियों को इतने दृढ़ रूप से अपने अधिकार में रखता है, अर्थात् यह धारणा कि वस्तुएँ ईश्वर से पृथक् अपने-आप में या अपने लिए अस्तित्व रखती हैं, अथवा प्रकृति के अधीन रहनेवाली कोई भी वस्तु स्वयमेव प्रेरित तथा परिचालित हो सकती है, उससे दूर हो गयी है, - यही उसके संदेह एवं विभ्रांति का तथा कर्म से इन्कार करने का कारण था।
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ।। २॥
२. हे कमल-लोचन श्रीकृष्ण! समस्त भूतों की उत्पत्ति और लय को मेरे द्वारा आप से विस्तारपूर्वक सुना गया है और आपके अविनाशी महात्म्य को भी सुना गया है।
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ।। ३।।
३. हे परमेश्वरा आपने अपने विषय में जैसा कहा है वह वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम! (फिर भी) मैं आपके ईश्वरीय दिव्य रूप और देह को देखना चाहता हूँ।
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ।। ४।।
४. हे प्रभो! यदि आप मानते हो कि आपका वह रूप मेरे द्वारा देखा जाना शक्य है तो, हे योगेश्वर ! आप अपने अविनाशी आत्म-स्वरूप का मुझे दर्शन कराइये।
वह जानता है कि दिव्य चेतन आत्मा का अक्षय महात्म्य ही इन सब बाह्य प्रतीतियों का रहस्य है।.... वह उनके गुणों के बारे में सुन चुका है तथा उनके आत्म-प्रकटीकरण के सोपानों तथा तरीकों को समझ चुका है; परन्तु अब वह इन योगेश्वर से अपने योग-चक्षु के सम्मुख अपनी उस वास्तविक अव्यय आत्मा को प्रकाशित करने के लिए कहता है। स्पष्ट ही उसका अभिप्राय उनके निष्कर्म अक्षरभाव की निराकार नीरवता से नहीं है, अपितु उन परमोच्च से है जिनसे ही समस्त शक्ति एवं कर्म उद्भूत होता है, सभी रूप जिनके आवरण हैं, जो विभूति में अपनी शक्ति प्रकाशित करते हैं, - जो कर्मों के स्वामी, ज्ञान और भक्ति के स्वामी, प्रकृति और उसके समस्त प्राणियों के परमेश्वर हैं। इस महत्तम सर्वग्राही दिव्यदर्शन के प्रीत्यर्थ प्रार्थना करने के लिए उसे प्रेरित किया गया है क्योंकि इस प्रकार ही उसे, जगत्कर्म में अपना भाग ग्रहण करने के लिए विश्व में अभिव्यक्त परमात्मा से आदेश प्राप्त करना होगा।
अर्जुन की वर्तमान मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी है जिसमें कि उसकी बुद्धि का भ्रम दूर हो चुका है। उसे यह भली-भाँति अनुभव हो गया है कि परमात्मा ही सभी कुछ के आदिकारण हैं, वे ही सभी कुछ के कर्ता-धर्ता हैं, उनके अतिरिक्त अन्य किसी चीज की कोई सत्ता ही नहीं है। और यह सत्य प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो इसके लिए विभूतियों के वर्णन से बुद्धि को और अधिक आधार प्राप्त होता है। परंतु फिर भी भौतिक इंद्रिय संवेदन तो हमें ऐसी पृथक्कारी सूचना देते ही रहते हैं कि जगत् में भित्र-भित्र तो हमें ऐसी जीव-जंतुओं का, पेड़-पौधों, पहाड़-नदियों आदि का भी उरावतत्व है। हालाँकि भीतर से भले ही यह बोध हो गया हो कि ये सभी परमात्मा के ही रूप हैं, तो भी भौतिक संवेदनों के अंदर ठोस रूप से यह विश्वास आ जाना आसान नहीं है। परंतु अर्जुन ने जिस स्थिति से आरंभ किया था उसमें तो वह विषाद और भ्रम में डूबा हुआ था। भगवान् उसकी शंकाओं आदि का समुचित उत्तर देते हुए धीरे-धीरे उसे इस स्थिति तक ले आए हैं कि अब उसका हृदय उनमें रस लेने लगा है, उसकी बुद्धि में प्रकाश आ गया है। तो फिर अब बाकी क्या है? बाकी है उसके इंद्रिय संवेदनों में प्रकाश लाना। बुद्धि के अंदर अनुभव होने के बाद भी यह भाव बना रहता है कि जिन चीजों की या विभूति आदि की बात की जा रही है वह एक गहरा सत्य तो है परंतु भौतिक रूप से तो उसे देख पाना कदाचित् ही संभव होता होगा। इसीलिए उसके अंदर यह इच्छा और जिज्ञासा जाग उठती है कि भगवान् अपने स्वरूप का जो वर्णन कर रहे हैं क्या वह उसके लिए गोचर होना संभव है। जैसे एक सच्चे प्रेमी भक्त का हृदय अपने प्रेमास्पद की चर्चा में गहरा आनंद अनुभव करता है वैसे ही अर्जुन भगवान् की विभूतियों के वर्णन में परम आनन्द अनुभव कर रहा है इसलिए उसमें प्रबल इच्छा जाग उठती है कि उसे वह सब दिखलाया जाए जिसका भगवान् वर्णन कर रहे हैं। दृष्टि एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण इंद्रिय है। किसी चीज के लिए अन्य इंद्रियों की सूचना के बाद भी दृष्टि के जुड़ने पर ही उसमें पूर्णता आती है। हमारी गहरी शक्तियों में भी स्मृति, श्रुति और दृष्टि का वर्णन आता है। इनमें भी दृष्टि अर्थात् सत्य के प्रकटन को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है।
प्रश्न : यहाँ पहले ही श्लोक में अर्जुन कहता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है परंतु अठारहवें अध्याय में भी अर्जुन कहता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है। तब फिर इनमें अंतर क्या है?
उत्तर : इसका कारण यह है कि साधना की किसी अवस्था विशेष में व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है। विश्वरूप दर्शन के बाद हृदय, बुद्धि, संवेदनों आदि भागों में अवश्य ही किसी सीमा तक तो विश्वास आ जाता है परंतु फिर भी जिस प्रकार का हमारा गठन है, उसमें इतने सब अनुभवों के बाद भी बुद्धि में कुछ भ्रम बाकी रह जाते हैं। इसीलिए अर्जुन इतने निरूपण के बाद भी कहता है कि गुणों के विषय में भगवान् ने वर्णन तो बहुत किया परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि वास्तव में गुण क्या हैं। उसी प्रकार वह कहता है कि आप 'अहं' 'माम्' आदि पदों का प्रयोग करते हैं, परंतु यह तो आप ने स्पष्ट ही नहीं किया कि आप कौन हैं, पुरुषोत्तम से आपका क्या संबंध है। पुरुष-प्रकृति के विषय में भी आपने चर्चा तो बहुत की है परंतु इनका वास्तविक मर्म क्या है। इस प्रकार अर्जुन के अंदर अभी कुछ प्रश्न हैं जिन्हें स्पष्ट किये जाना बाकी है। इसलिए किसी भाग में तो उसका मोह नष्ट हो गया है परंतु इन सभी बचे प्रश्नों के हल होने के बाद ही वह अठारहवें अध्याय में कहता है कि उसका मोह नष्ट हो चुका है।
श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।। ५।।
५. श्रीभगवान् ने कहाः हे पार्थ! मेरे नाना प्रकार के और नाना रंग और आकार वाले सैंकड़ों और सहस्रों दिव्य रूपों को देख।
पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्वर्याणि भारत ।। ६।।
६. हे भारत! आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और मरुद्गणों को देख; और बहुत से ऐसे आश्चयों को देख जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है।
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि ।। ७।।
७. हे गुडाकेश (निद्राविजयी अर्जुन)! आज यहाँ मेरे शरीर में ही सभी चर और अचर सहित संपूर्ण जगत् को एकीभूत हुआ देख, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी देखना चाहता है वह भी देख।
इस प्रकार यही इस (विश्वरूपदर्शन) की मुख्य बात तथा केंद्रीय मर्म है। यह अनेक में 'एक' तथा 'एक' में अनेक का दर्शन है, - और सभी कुछ वह 'एक' ही हैं। यही वह दर्शन है जो दिव्य योग के चक्षु के लिए वह सब जो है और जो था और जो होने वाला है उस सब को मुक्त कर देता है, उसका औचित्य सिद्ध करता तथा उसकी व्याख्या करता है। एक बार यह दर्शन प्राप्त हो जाने तथा इसे धारण कर लेने पर यह ईश्वर की उज्ज्वल कुल्हाड़ी से सब संशयों तथा व्यग्रताओं की जड़ पर कुठाराघात करता है और सब निषेधौम् विरोधाभासों को जड़ से मिटा देता है। यह वह दर्शन है जो समन्वित एकीभूत करता है। यदि जीव इस दर्शन में परमात्मा के साथ एकत्व साथित क सके, - अर्जुन अभी तक इसे नहीं प्राप्त कर सका है, इसलिये हम देखते है दर्शन करने पर वह भयभीत होता 3 - a इस संसार में जो कुछ भी पर्वका दर्शन करके उसके लिए संत्रास नहीं रह जाता। हम देखते हैं कि यह भी परीक का ही एक रूप है और एक बार जब हमने, उसे केवल अपने-आप में होन देखते हुए, उसके अन्दर उनके प्रयोजन को ढूँढ़ लिया होता है, तब हम समा जगत् को सर्वसमावेशी हर्ष तथा प्रबल साहस के साथ स्वीकार कर सकते हैं अपने नियत कर्म की ओर सुनिश्चित पगों से अग्रसर हो सकते हैं और उससे परमोच्च परिणति की परिकल्पना कर सकते हैं।
दर्शन करने पर अर्जुन भयभीत इसलिए होता है क्योंकि अभी भी उसमें अहंबोध, अपनी पृथक् सत्ता का बोध है और जब तक पृथक्ता का बोध होता है तब तक तो भय बना ही रहता है।
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८॥
८. परन्तु अवश्य ही तू अपनी इन आँखों से मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ उससे तू मुझे मेरे ईश्वरीय योग में देख।
सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ।। ९।।
९. सञ्जय ने कहाः हे राजन्! ऐसा कह कर महायोगेश्वर श्रीहरि (श्रीकृष्ण) ने अर्जुन को अपने परम ईश्वरीय रूप को दिखलाया।
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ।। १०।।
१०. अनेक मुखों और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत झाँकियों वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित, युद्ध के लिए उद्यत अनेक आयुधों से सुसज्जित।
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्वाश्वर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ।। ११ ।।
११. दिव्य मालाओं और वखों को धारण किये हुए, दिव्य गंधों के अनुलेपन है। सुगन्धित, अनन्त और समस्त आश्चयों से परिपूर्ण देव जिनके मुख सर्वत्र हैं।
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२॥
१२. यदि आकाश में सहस्रों सूयाँ की ज्योति एक साथ जगमगा उठे तो वह ज्योति कदाचित् उस महापुरुष के देह की ज्योति के सदृश हो।
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ।। १३।।
१३. वहाँ उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुन ने सम्पूर्ण विश्व को उसके अनेकविध विभागों में होते हुए भी उसे देवों के परमदेव के उस शरीर में एकीभूत अवस्था में देखा।
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ।
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ।। १४।।
१४. तब विस्मय से अभिभूत, रोमांचित देहवाले उस धनञ्जय (अर्जुन) ने देव के समक्ष शीश नवाते हुए और हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहा।
अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ।। १५।।
१५. अर्जुन ने कहाः हे देव! मैं समस्त देवों को और विभिन्न जाति के जीवों के समूहों को, कमलरूप आसन पर बैठे हुए सृष्टिकर्त्ता प्रभु ब्रह्मा को और समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को आपकी देह में देखता हूँ।
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।। १६ ।।
१६. सभी ओर अनंत रूपों वाले आपको मैं असंख्य भुजाओं, उदरों, नेत्रों और मुखों से युक्त देखता हूँ; किन्तु हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप! मैं आपका आदि, मध्य और अंत नहीं देखता।
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीसानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ।। १७।।
१७. मैं आपको मुकुट से सुशोभित, गदा और चक्र से सुसज्जित देखता हूँ, आपको देख पाना या पहचान पाना कठिन है क्योंकि आप एक देदीप्यमान तेज के पुंज हैं, सब ओर से व्याप्त करने वाली ज्वाला हैं, अग्नि और सूर्य के समान चमकदार अपरिमेय हैं जो मुझे सब ओर से घेरे हुए हैं।
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।। १८॥
१८. आप हमारे लिये ज्ञातव्य परम अक्षर ब्रह्म हैं, आप इस विश्व के उच्च आधार और निधान हैं, आप सनातन नियमों के अविनाशी संरक्षक हैं, आप सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है।
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ।। १९।।
१९. आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनन्त बलयुक्त, असंख्य भुजाओंवाला देखता हूँ, आपके नेत्र चन्द्र और सूर्य हैं, आपका मुख प्रज्ज्वलित अग्नि के समान है, आपके निज तेज की ज्वाला से आपको इस संपूर्ण विश्व को तपाता हुआ देखता हूँ।
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।
दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ।। २० ।।
२०. हे महात्मन् ! द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच का सब प्रदेश और समस्त दिशाएँ एकमात्र अकेले आप से ही व्याप्त हैं; आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं।
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।। २१॥
२१. देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं; कोई-कोई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं; महर्षि और सिद्धों के समुदाय "शांति हो, कल्याण हो" ऐसा कहते हुए अनेक प्रकार के स्तुतिवचनों से आपकी स्तुति कर रहे हैं।
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्वोष्मपाश्च ।
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताचैव सर्वे ॥ २२॥
२२. रुद्र और आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेवाः, दो अश्विनीकुमार, मरुत् और पितरों का समुदाय (ऊष्मपाः) और गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह हैं, सभी की दृष्टि विस्मित होकर आपको देख रही है।
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ।। २३ ।।
२३. हे महाबाहो । आपके बहुत से मुखों और नेत्रों, अनेक भुजाओं, जंघाओं, पैरों और उदरोंवाले, कराल दाढ़ों से युक्त आपके भयानक विराद् रूप को देखकर समस्त लोक भय से कम्पित और व्यथित हो रहे हैं और मैं भी कम्पित और व्यथित हो रहा हूँ।
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीसविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ।। २४।।
२४. हे विष्णो! आकाश को स्पर्श करते हुए, अनेक रंगों में जाज्वल्यमान, खुले हुए मुखोंवाले, बड़े-बड़े आग्नेय नेत्रों वाले आपको मैं देखता हूँ। मेरा मन अत्यधिक व्यथित है और मुझे शान्ति या धैर्य भी नहीं है।
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। २५।।
२५. भयंकर दाढ़ों के कारण विकराल और मृत्यु तथा काल की अग्नि के समान आपके मुखों को जब मैं देखता हूँ तो मैं दिशाओं का बोध खो बैठता हूँ और मैं शांति अनुभव नहीं करता। हे देवों के देव, जगत् के आश्रय! आप प्रसन्न हों।
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः ।
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ।। २६ ।।
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ।। २७॥
२६-२७. राजाओं और वीरों के समूहों तथा भीष्म और द्रोण तथा कर्ण के सहित ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, तथा हमारे भी प्रधान-प्रधान योद्धा तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ोंवाले अति भयंकर जबड़ों (मुखों) में प्रवेश कर रहे हैं; और कुछ आपके दाँतों के बीच में चकनाचूर हुए सिरोंवाले दिखायी दे रहे हैं।
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।। २८॥
२८. जिस प्रकार नदियों के बहुत से जलों के प्रवाह (धाराएँ) समुद्र की ओर दौड़ते हुए उसमें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये सब मानवलोक के शूरवीर आपके अनेक ज्वलंत मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।
तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ।। २९।।
२९. जिस प्रकार पतंगे मरने के लिये तीव्र वेग के साथ प्रज्ज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये सब मनुष्य भी मरने के लिये तीव्र वेग के साथ आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ध्वलद्भिः ।
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ।।३० ।।
३०. हे विष्णो ! आप समस्त लोकों को अपने प्रज्ज्वलित मुखों से सब और से ग्रसित करते हुए चाट रहे हो; संपूर्ण जगत् आपके जाज्वल्यमान तेज से परिपूर्ण है और उग्र प्रभाओं से तप रहा है।
[यह परम और विश्वपुरुष का] वह रूप है जिससे मनुष्य का मन जानबूझ कर दूर हट जाता है और शुतुरमुर्ग की भाँति अपना सिर छुपा लेता है ताकि स्वयं उन 'रौद्र' या 'भयंकर' को न देख पाने के कारण कदाचित् उनकी भी नजर में न आये। दुर्बल मानव हृदय केवल अनुकूल तथा सुखद सत्यों को ही चाहता है या फिर उनके अभाव में रुचिकर गाथाओं को ही पसंद करता है। वह सत्य को उसकी समग्रता में नहीं प्राप्त करना चाहता, क्योंकि सत्य में ऐसा बहुत कुछ है जो स्पष्ट, रुचिकर तथा सुखद नहीं है, इतना ही नहीं, बल्कि जिसे समझना कठिन है तथा सहन करना और भी भारी है। अपरिपक्व धर्मवादी, सतही आशावादी विचारक, भावुक आदर्शवादी, अपने भावों तथा संवेदनों की दया पर आश्रित मनुष्य विश्व-सत्ता के कठोरतर परिणामों तथा निष्ठुर और उग्रतर रूपों को तोड़-मरोड़कर उनसे बच निकलने में सहमत हैं। छिपने-बचने के इस सामान्य खेल में भाग न लेने के कारण भारतीय धर्म को अज्ञानपूर्वक निन्दा की गयी है, क्योंकि, इसके विपरीत, उसने परमेश्वर के रौद्र, भयानक तथा मधुर और सुन्दर प्रतीकों को साथ-साथ निर्मित किया और अपने सामने रखा है। क्योंकि यह उसके सुदीर्घ चिंतन तथा आध्यात्मिक अनुभव की गंभीरता तथा विशालता ही है जो उसे इन कमजोर जुगुप्साओं को अनुभव करने या इनको स्वीकृत करने से रोकती है।
भारतीय संस्कृति का यह एक ऐसा गंभीर सत्य है जिसे समुचित रूप से समझ लेना अत्यावश्यक है क्योंकि यदि इसे न समझें तो हम संसार को भी नहीं समझ सकते और इस कारण विचलित स्थिति में ही रहते हैं। उदाहरण के लिए, साधक के मन में यह भाव उठता है कि श्रीमाताजी परम दयालु हैं और सभी कुछ उनकी कृपा की ही अभिव्यक्ति है और जो कुछ भी वे करती हैं वह केवल कल्याण के लिए ही करती हैं। सभी आध्यात्मिक जन इसी प्रकार की बातें करते हैं। परंतु भारतीय संस्कृति में ही यह विशिष्टता रही है जो जगज्जननी को कल्याणकारी माता ही नहीं अपितु संहाररत नरमुण्डधारी काली के रूप में भी पूजने का साहस रखती है। हमारी संस्कृति भगवान् के समग्र रूप को स्वीकार करने का साहस रखती है क्योंकि यदि भगवान् को उनके केवल किन्हीं एकांगी रूपों में ही स्वीकार किया जाए और उनके दूसरे पक्षों को अस्वीकार कर दिया जाए, उनके प्रति जुगुप्सा का भाव रखा जाए तब तो किसी प्रकार की समग्र दिव्यता का साक्षात्कार तो संभव ही नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार का यह संसार है इसमें बहुत सारी चीजें आपस में घुल-मिल गई हैं। यहाँ सत्य और मिथ्यात्व, शुभ और अशुभ, प्रकाश और अंधकार आदि सभी साथ-साथ अभिव्यक्त हो रहे हैं, आसुरी शक्तियों और दैवी शक्तियों के बीच भयंकर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इसलिए भले ही यह किसी स्तर पर तो मूलतः सत्य है कि सब कुछ भगवान् की ही इच्छा से होता है परंतु वास्तविक अभिव्यक्ति में सब कुछ सही नहीं है, चीजें अपने यथास्थान पर नहीं हैं। और इन सब विषमताओं का, आसुरी शक्तियों का सामना करने और उनका विनाश करने के लिए महाकाली की परम आवश्यकता है। इसलिए प्रतीति में अवश्य ही वे रौद्र रूपा हैं परंतु उनकी क्रिया परम कल्याणकारी है क्योंकि वे एक ही वार में भीतरी और बाहरी शत्रुओं का नाश कर डालती हैं। जो चीजें हमें सुदीर्घ काल से बाँधे हुए थीं या जो हमें सुदीर्घ काल तक बाँध सकती थीं, उन सभी का उनके एक ही वार से नाश हो जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, तब यह अनिष्ट इस पर निर्भर करता है कि हमारा तादात्म्य किससे है। यदि हमारा तादात्म्य अपने मन, प्राण और शरीर से ही है तब तो हमारा अनिष्ट कभी भी हो सकता है परंतु यदि हमारा तादात्म्य अपनी आत्मा से है तब उसका कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी सत्य की उपयुक्तता या उसकी सत्यता इस पर निर्भर करती है कि हम उसे प्रयुक्त किस प्रकार कर रहे हैं। इसलिए सभी चीजें हमारी अंतरात्मा के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम होती हैं न कि हमारी बाहरी सत्ता के दृष्टिकोण से। और वास्तव में जो हमारी आंतरिक सत्ता के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम होता है वही सच्चे रूप में हमारी बाहरी सत्ता के लिए भी उत्तम हो सकता है। इसीलिए परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना अच्छा है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है; परमात्मा के समीप जाना और भी अच्छा है, परंतु यह भी पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता तो इस बात की है कि व्यक्ति परमात्मा के राज्य की स्थापना के लिए उनके पक्ष में खुलकर संघर्ष करने के लिए तैयार रहे क्योंकि इस जगत् में दैवीय और आसुरी शक्तियों के बीच संघर्ष चलता है और व्यक्ति को सक्रिय रूप से दैवीय शक्तियों के पक्ष में युद्ध करना ही होगा। हमारे जितने भी अवतार और महापुरुष आदि आए हैं सभी ने अपने जीवन में भागवत् साम्राज्य की स्थापना के लिए घोर संघर्ष किया है। और इसी कारण श्रीअरविन्द इस अध्याय के आरंभ में ही कहते हैं कि, "विश्व-पुरुष का दर्शन गीता के उन सुप्रसिद्ध प्रकरणों में से है जो अत्यंत ओजस्वी रूप में काव्यमय हैं, परन्तु गीता की विचारधारा में इसका स्थान सर्वथा सतह पर प्रकट नहीं है।" सतह पर यह प्रकट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ केवल दैवीय ही नहीं अपितु आसुरी शक्तियाँ भी हैं और उनका सामना करना ही होगा, उनके साथ युद्ध करना होगा। इसलिए हमें भगवान् के सौम्य रूप को हो नहीं अपितु उनके रौद्र रूप को भी बिना किसी भय और जुगुप्सा के स्वीकार करना ही होगा। जब तक आसुरी चीजों का बोलबाला है तब तक तो दुर्गा के रौद्र रूप की, काली के अट्टहास की परम आवश्यकता है। और वास्तव में तो इनके रौद्र रूप में ही इनका परम कल्याण भी छिपा है। यदि हम संसार में विभिन्न शक्तियों की क्रिया को समुचित और समग्र रूप से देख पाएँ तो इसके अंदर ईश्वर के सभी पक्षों की क्रिया को भी समुचित रूप से देख पाएँगे अन्यथा तो हम सदा ही भगवान् को समग्रता में न देखकर किसी एक पक्ष से ही देखेंगे और उनकी समग्र क्रिया से चूक जाएँगे। जो धर्म भगवान् के रौद्र रूप को देखने का साहस नहीं कर सकते उन्हें फिर चीजों के स्पष्टीकरण के लिए किसी शैतान की परिकल्पना करनी पड़ती है। तब वे कहते हैं कि भगवान् तो कल्याणकारी ही हैं परंतु शैतान भी है जो सभी वीभत्स चीजों का कारण है। परंतु भारतीय आध्यात्मिकता का कभी भी ऐसा कोई एकांगी दृष्टिकोण नहीं रहा।
भारतीय आध्यात्मिकता जानती है कि ईश्वर परम प्रेम, शान्ति, स्थिरता और शाश्वतता हैं, - गीता, जो हमारे समक्ष इन भयंकर रूपों को प्रस्तुत करती है, उन परमेश्वर को, जो उन भयंकर रूपों को धारण करते हैं उनका, सर्वभूतों के सखा और प्रेमी के रूप में भी वर्णन करती है। परन्तु उनका जगत् के दिव्य शासन के रूप में एक अधिक कठोर पहलू भी है, जो आरम्भ से ही हमारे सम्मुख उपस्थित रहता है, वह है संहार का पहलू, और उसकी उपेक्षा करना भागवत् प्रेम, शान्ति, स्थिरता और शाश्वतता के पूर्ण सत्य से वंचित होना है और यहाँ तक कि इस पर आंशिकता तथा भ्रम का रूप थोप देना है, क्योंकि जिस केवल सुखप्रद रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है, वह जिस जगत् में हम रहते हैं उसकी प्रकृति के द्वारा प्रमाणित नहीं होता। हमारा यह संघर्षात्मक तथा प्रयासमय जगत् भयंकर, खतरनाक, विनाशकारी, भक्षक जगत् है जिसमें जीवन बड़े जोखिम भरे ढंग से रहता है, तथा मनुष्य की देह और आत्मा अतिविकराल संकटों के बीच विचरण करते हैं, यह एक ऐसा जगत् है जिसमें आगे उठाये जानेवाले प्रत्येक कदम के द्वारा, हम चाहें या न चाहें, कुछ-न-कुछ कुचला जाता है और टूट जाता है, जिसमें जीवन का प्रत्येक श्वास मृत्यु का भी प्रश्वास है। जो कुछ भी हमें अशुभ या भीषण प्रतीत होता है उस सब के लिए एक अर्द्ध-सर्वशक्तिमान शैतान को उत्तरदायी ठहराना या उसे प्रकृति का अंग कहकर एक ओर रख देना और इस प्रकार जगत्-प्रकृति तथा ईश्वर-प्रकृति में अलंघ्य विरोध खड़ा कर देना, मानो प्रकृति ईश्वर से स्वतंत्र हो, अथवा उस सबके लिए मनुष्य व उसके पापों को उत्तरदायी ठहराना, मानो इस जगत् के निर्माण में उसकी आवाज का बड़ा भारी महत्त्व हो या वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी रच सकता हो, - ये सब ऐसी अनाड़ी ढंग की सुविधाजनक युक्तियाँ हैं जिनका भारत की धार्मिक विचारधारा ने कभी आश्रय नहीं लिया। हमें यथार्थता को साहस के साथ आँख में आँख डालकर देखना होगा और यह देखना होगा कि परमेश्वर ने ही, और किसी ने नहीं, अपनी सत्ता के अन्दर इस जगत् का निर्माण किया है और उन्होंने इसे इस प्रकार का ही बनाया है। हमें देखना होगा कि अपनी संतानों को निगलनेवाली प्रकृति, प्राणियों के जीवनों को हड़प जानेवाला काल, अटल तथा सार्वभौम मृत्यु, तथा मनुष्य और प्रकृति में निहित हिंसक रुद्र शक्तियाँ भी, अपने एक अन्य वैश्व रूप में, वह परमोच्च ईश्वर ही हैं। हमें देखना होगा कि वे उदार तथा मुक्तहस्त स्रष्टा, सर्वसहायक, शक्तिमान् और दयालु जगत्पालक ईश्वर ही भक्षक तथा संहार' ईश्वर भी हैं... केवल तभी जब हम पूर्ण ऐक्य की दृष्टि से देखते हैं और इस सत्य को अपनी सत्ता की गहराइयों में अनुभव करते हैं, तभी हम उस मुखौटे या छद्मरूप के पीछे भी सर्वानंदमय परमेश्वर के शांत और सुन्दर मुख को पूर्ण रूप से पा सकते हैं और इस स्पर्श में, जो हमारी अपूर्णताओं की कसौटी है, मनुष्य की आत्मा के सखा और निर्माता का स्पर्श पा सकते हैं। जगतों की विसंगतियाँ ईश्वर की ही विसंगतियाँ हैं और केवल उन्हें स्वीकार करके तथा उनमें से होकर आगे बढ़ने से ही हम उनके परम सामंजस्य की महत्तर सुर-संगतियों तक तथा उनके विश्वातीत और विश्वगत आनंद के शिखरों और हर्ष-रोमांचित विशालताओं तक पहुँच सकते हैं।
गीता ने जो समस्या उठायी है तथा जो समाधान दिया है वे विश्व-पुरुष के दर्शन के इसी स्वरूप की माँग करते हैं।... जब उसका [अर्जुन का] इस सत्य के मूर्तिमंत रूप से साक्षात्कार कराया जाता है, वह उसके अंदर भागवत् महात्म्य की छवि के द्वारा त्रास तथा संहार के इस रूप को अतिशय रूप से परिवर्धित देखता है और भयभीत हो उठता है तथा उसे सह नहीं सकता। क्योंकि, सर्वात्मा को अपने-आप को प्रकृति के अन्दर इस रूप में प्रकट ही क्यों करना चाहिए? आखिर अभिप्राय क्या है इस मृत्युशील सत्ता का जो कि एक सृष्टिकारी तथा सर्वग्रासी ज्वाला है, इस विश्वव्यापी संघर्ष तथा इन सतत् विनाशकारी सृष्टिचक्रों का और प्राणियों के इस प्रयास, व्यथा, वेदना तथा विनाश का? वह इस पुरातन प्रश्न को पूछता है तथा सनातन प्रार्थना को व्यक्त करता है...
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ।। ३१।।
३१. इस भयानक रूप को धारण करनेवाले आप कौन हैं यह मुझे बतलाइये हे देवों में श्रेष्ठदेव! आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हों। आप जो आदि से हैं, आपको मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तियों के पीछे के मूल संकल्प को नहीं जानता।
भगवान् उत्तर देते हैं कि 'संहार' ही मेरी क्रिया-प्रवृत्तियों का मूल संकल्प है जिसे लेकर मैं यहाँ कुरुक्षेत्र के इस मैदान में स्थित हूँ... यह एक विश्वव्यापी संहार है जो कालपुरुष की प्रक्रिया में आ उपस्थित हुआ है। 'मेरा एक पूर्वदर्शी प्रयोजन है जो अपने आप को अमोघ रूप से चरितार्थ करता है और किसी मनुष्य की उसमें सहभागिता या उससे परिहार न उसे रोक सकता, न बदल सकता और न पलट ही सकता है;
______________________________
*क्या तुम अपने मृत्यु के क्षण में या पीड़ा की घड़ियों में भी अपने उत्पीड़क और अपने संहारक में ईश्वर को देख पाते हो? क्या तुम उस ईश्वर को उस में देख पाते हो जिसका तुम संहार कर रहे हो, और क्या 'उसे' उस समय भी देख और प्रेम कर पाते हो जब तुम संहार कर रहे होते हो? तो तुमने परम ज्ञान पा लिया है। वह कृष्ण को कैसे पा सकता है जिसने कभी काली को न पूजा हो?
मनुष्य के द्वारा इस भूतल पर किंचित्मात्र भी किये जा सकने से पहले ही सभी कुछ मेरे द्वारा अपने संकल्प की सनातन दृष्टि में सम्पन्न किया जा चुका होता है। काल-रूप में मुझे पुरानी रचनाओं को नष्ट करना तथा नये, महान् और श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करना है। तुझे दिव्य शक्ति तथा प्रज्ञा के मानवीय यंत्र के रूप में इस युद्ध में, जिसे तू रोक नहीं सकता, सत्य के लिए लड़ना तथा इसके विरोधियों का वध करना और उन्हें जीतना है।
श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धोलोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।। ३२।।
३२. श्रीभगवान् ने कहाः मैं लोकों का विनाश करनेवाला कालपुरुष हूँ, जो यहाँ लोकों के विनाश में प्रवृत्त विकराल रूप धारण किये हुए है। प्रतिपक्षी सेनाओं में जो योद्धा उपस्थित हैं वे सब तेरे युद्ध किये बिना भी नहीं बचेंगे।
ये काल तथा विश्व-पुरुष के रूप में प्रकट कालातीत ही हैं जिनसे कर्म का आदेश प्रादुर्भूत हुआ है। क्योंकि, निश्चय ही जब भगवान् यह कहते हैं कि "मैं भूतों का क्षय करने वाला काल हूँ,” तब उनके कहने का तात्पर्य यह नहीं होता कि वे केवल काल-पुरुष ही हैं या काल-पुरुष का सम्पूर्ण अर्थ संहार ही है। परंतु यही उनके कार्यों की वर्तमान प्रवृत्ति है। संहार सदा ही सृष्टि के साथ-साथ चलनेवाला या बारी-बारी से आनेवाला तत्त्व है और संहार करके तथा नये सिरे से रचना करके ही जीवन के स्वामी जगत् के प्रतिपालन का अपना सुदीर्घ कार्य सम्पन्न करते हैं।...जो कोई भी युद्ध और संहार के इस विधान से छुटकारा पाने के लिए समय से पूर्व यत्न करता है वह विश्व-पुरुष के महत्तर संकल्प के विरुद्ध एक व्यर्थ की चेष्टा करता है। जो कोई अपने निम्नतर अंगों की दुर्बलता के कारण उससे पीठ फेरता है, जैसा कि अर्जुन ने आरम्भ में किया, वह उस सच्ची वीरता को नहीं अपितु प्रकृति के तथा कर्म और जीवन के कठोरतर सत्यों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक साहस के अभाव को ही दिखला रहा होता है। मनुष्य युद्ध के नियम का अतिक्रम के अभाव क्ता के महत्तर विधान को उपलब्ध करके ही कर सकता है... तथ तक सच्ची शांति नहीं हो सकती जब तक कि मनुष्य का हृदय शांति का अधिकारी नहीं होता; विष्णु का विधान तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि रुद्र का ऋण नहीं चुका दिया जाता। ऐसी अवस्था में युद्ध से मुँह मोड़ कर अब तक अविकसित मानवजाति को क्या प्रेम तथा एकता के नियम का उपदेश देना होगा? प्रेम और एकत्व के विधान के शिक्षकों का होना आवश्यक है, क्योंकि केवल उसी तरीके से अंतिम उद्धार की प्राप्ति हो सकती है। परंतु जब तक काल-पुरुष मनुष्य के अंदर तैयार नहीं हो जाता तब तक आंतरिक एवं चरम सत्य बाह्य एवं तात्कालिक सत्य पर प्रभुत्व नहीं प्राप्त कर सकता। ईसा और बुद्ध आये और चले गये, परंतु रुद्र ही हैं जो अब तक भी जगत् को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इस बीच मानवजाति का प्रचंड अग्र प्रयास, जो कि अहंभावपूर्ण शक्ति से अत्यधिक लाभ उठानेवाली शक्तियों तथा उनके दासों के द्वारा व्यथित तथा उत्पीड़ित है, संघर्ष के वीरनायक की तलवार तथा इसके पैगंबर की वाणी के लिए पुकार रहा है।
जहाँ भी कहीं अपूर्णता है, स्वार्थपरता है, क्षुद्रता है उस सब पर रुद्र अपना प्रहार करते हैं और उसे मिटा डालते हैं। इसीलिए रौद्र रूप संहार करने वाला बताया गया है। वेदों में भी रुद्र का प्रतीक आता है जो अपने प्रहार से हमें हमारी क्षुद्र आदतों से, निम्न कामनाओं, वासनाओं, सुख-भोग की लालसाओं से, जो कि हमें जीवन भर जकड़े रखती हैं, मुक्त कर देते हैं। इसलिए जिस प्रकार की वर्तमान पार्थिव स्थिति है उसमें अन्य देवताओं की क्रिया समुचित रूप से हो पाए उससे पहले रुद्र की क्रिया आवश्यक है। वर्तमान अवस्था में तो व्यक्ति इतनी पाशों में बँधा है कि किसी प्रकार की मुक्त क्रिया करने की तो वह सोच ही नहीं सकता। इसलिए वह मुक्त क्रिया कर पाए उसके लिए पहली आवश्यकता है कि उसकी सभी पाशें काट दी जाएँ, और रुद्र यही करते हैं। महाकाली भी यही करती हैं। वे अपने एक ही वार से हमारे जन्म-जन्मांतरों के बंधन काट डालती हैं। इसीलिए वे परम कल्याणमयी हैं।
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्मुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्।
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ।। ३३॥
३३. इसलिये तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, तेरे शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग कर। मेरे द्वारा ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, अतः हे सव्यसाचिन् अर्जुन । तू तो निमित्तमात्र बन जा।
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योषवीरान् ।
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्।। ३४ ।।
३४. जो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं उन द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धाओं को मार; संत्रप्त और व्यथित मत हो। युद्ध कर, तू रण में शत्रुओं को जीतेगा।
उस महान् तथा घोर कर्म के फल का वचन दे दिया गया है और उसके संबंध में भविष्यकथन कर दिया गया है, पर यह ऐसा फल नहीं है जिसके लिए व्यक्ति लालायित हो, क्योंकि उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, - अपितु ऐसा फल है जो भगवदिच्छा के परिणाम के रूप में, संपन्न किये जाने योग्य कार्य के यश और सफलता के रूप में, भगवान् के द्वारा अपनी विभूति के अन्दर अपने-आप को ही प्रदान किये जानेवाले यश के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार जगत्-संग्राम के नायक को कर्म के लिए अंतिम तथा अलंघ्य आदेश दे दिया गया है।
अर्जुन को अब अलंघ्य आदेश प्राप्त हो चुका है, ऐसा आदेश जिसकी अवहेलना या अनदेखी नहीं की जा सकती। स्वयं श्रीअरविन्द को अपने भीतर से चंदेर नगर जाने का ऐसा ही अलंघ्य आदेश प्राप्त हुआ था। अपनी एक पुस्तक में श्रीअरविन्द ने इस पूरे वृत्तांत का वर्णन किया है कि किस प्रकार लगभग असंभव परिस्थितियों में वे उस आदेश की पालना करते हुए वहाँ पहुँचे। पूरा वृत्तांत बहुत रोमांचक है कि यदि कहीं भी कोई चूक हो जाती तो यह पूरी संभावना थी कि उन्हें पकड़ कर कारावास में डाल दिया जाता। इससे यह पता लगता है किस प्रकार आदेश के साथ ही साथ भगवान् की कृपा छोटे से छोटे ब्यौरे की भी इतने सटीक रूप से व्यवस्था करती है जितनी कि कोई मनुष्य अपने सामर्थ्य के सहारे करने की सोच भी नहीं सकता। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी भीतर के उस आदेश पर, उस वाणी पर संदेह नहीं हुआ कि उस वाणी के आधार पर ही उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया तब श्रीअरविन्द कहते हैं कि वह वाणी या वह आदेश ऐसा था कि उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था।
प्रश्न : भगवान् अर्जुन को कहते हैं कि मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं तू तो केवल निमित्तमात्र बन, तो इसका अर्थ क्या है?
उत्तर : हमारा यह जगत् तो जगत् श्रृंखला में निचले स्तर पर है। हमारे ऋषियों ने पहले ही इसका अनुभव प्राप्त कर लिया था कि इस जगत् में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो सकता जो पहले से कहीं घटित न हुआ हो। इसी कारण तो हम भविष्यकथन कर सकते हैं। श्रीमाताजी को इन जगत् श्रृंखलाओं का और इनकी क्रिया का गहरा ज्ञान था। इसलिए श्रीअरविन्द के साथ चर्चा में वे उन्हें जब आवश्यक होता था तब बताती थीं कि कौनसी चीजों में अभिव्यक्ति से पूर्व हस्तक्षेप करके उनके क्रम में फेरबदल किया जा सकता है, कौनसी ऐसी घटनाएँ हैं जो इस जगत् अभिव्यक्ति के इतनी निकट आ चुकी हैं कि अब उनमें हस्तक्षेप को अधिक संभावनाएँ नहीं हैं। श्रीअरविन्द की सेवा में नियुक्त कुछ अंतरंग भक्तों के साथ उनकी चर्चा-परिचर्चा के अभिलेखों से हमें पता लगता है कि किस प्रकार विश्व युद्ध के समय श्रीमाताजी की सहायता से श्रीअरविन्द विश्व घटनाओं में अपनी योगशक्ति द्वारा हस्तक्षेप कर के उन्हें दिशा प्रदान कर रहे थे। कुछ मामलों में तो उन्होंने सुदूर देशों में बैठे राजनेताओं के पूरे के पूरे भाषण को ही अपने अनुरूप शब्द प्रदान किये जिसके विषय में स्वयं वे राजनेता भी सचेतन नहीं थे। अपने एक भाषण में चर्चिल कुछ इस प्रकार कहते हैं कि कई बार उन्हें बड़े प्रबल रूप से यह महसूस होता है कि कोई शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही है और वह तब तक उनका साथ नहीं छोड़ेगी जब तक कि वे एक सही उद्देश्य के पक्ष में खड़े रहेंगे।
अब इससे एक प्रश्न और उठता है कि क्या सभी कुछ पूर्वनियत होता है या फिर हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा संभव है? श्रीमाताजी कहती हैं कि जो कुछ भी घटित होना हो वह किसी स्तर पर पूर्व में घटित हो चुका होता है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। यदि हम एक स्थान से किसी दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे हों तो मार्ग में आने वाली चीजें भले हो पहले से विद्यमान होती हैं, परंतु हमारे लिए उनकी विद्यमानता तब आती है जब वे हमें गोचर होती हैं। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति वहाँ जो कुछ भी देखता है वह भले ही पहले से विद्यमान होता है परंतु उसकी चेतना के लिए वह अस्तित्व में तब आता है जब वह उसे देखता है। वहीं यदि साथ ही गंतव्य तक पहुँचने के अनंत मार्ग हों, तब तो हमारे सामने जो-जो दृश्य आने हैं वे तो हमारे लिए सर्वथा अप्रत्याशित ही होंगे। साथ ही हमें मार्ग के चयन की स्वतंत्रता होती है। और जिस मार्ग का हम चयन करते हैं उसके अनुसार ही दृश्य हमारे सामने आते हैं। इस तरीके से हम इसे एक अर्थ में स्वतंत्र इच्छा कह सकते हैं और एक अर्थ में पूर्वनिर्धारित भी कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें यह भान भी होना चाहिये कि हमारा स्वतंत्रता का बोध तो सही है परंतु यह स्वतंत्रता हमारी आत्मा के लिए है न कि हमारे बाहरी भागों के लिए। प्रायः ही हम यह भूल कर बैठते हैं और वही सभी भ्रांतियों का कारण बन जाती है। स्वतंत्रता हमारी आत्मा को होती है जबकि हमारे बाहरी भाग तो अपने-अपने विधानों में बद्ध हैं। इसलिए जिस अनुपात में हम अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होते हैं उस अनुपात में हम स्वतंत्र होते हैं और जिस हद तक हम अपने निम्नतर और बाहरी भागों से संयुक्त होते हैं उस हद तक बद्ध होते हैं। अब चूँकि हम पूर्णतया जड़ नहीं हैं इसलिए हमें कुछ-कुछ स्वतंत्रता का भान होता है। परंतु चूंकि हम अपनी आत्मा से दूर होते हैं इसलिए यह स्वतंत्रता का भान भी अपूर्ण ही होता है। दूसरे, जो बाहरी घटनाएँ भी हमारे साथ होती हैं, भले ही हमारे दृष्टिकोण से प्रिय हों या अप्रिय, परंतु एक गहरे दृष्टिकोण से वे सारी इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी आत्मा ने उन परिस्थितियों का, उन घटनाओं का चयन किया होता है। यदि वह ऐसा चयन न करे तो उसके साथ वे घटनाएँ घटित न होकर दूसरी वे घटित होंगी जिनका वह चयन करेगी। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम इस गुत्थी पर कुछ अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। यदि पेड़ से कोई फल गिरता है तो उसकी नियति है नीचे जमीन पर गिरना। परंतु कोई मानसिक चेतना हस्तक्षेप करके उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ कर उसकी नियति बदल सकती है। अतः चेतना के स्तरक्रम की अनंत श्रृंखला है और एक स्तर की नियति को उससे उच्चतर स्तर के हस्तक्षेप के द्वारा बदला जा सकता है। अब इसमें कोई यह तर्क दे सकता है कि परम दिव्य विधान में वह हस्तक्षेप भी पूर्वनियत था। परंतु वहीं एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी है जो कहता है कि चूंकि यह आत्मा की इच्छा थी इसलिए उस इच्छा के अनुसार ही जो-जो हस्तक्षेप आवश्यक थे वे होते हैं और अभीष्ट परिणाम के लिए हस्तक्षेपों का क्रम भी बदल सकता है। परंतु अंततः होता वही है जो आत्मा की, हमारे अंदर बैठे परमात्मा की इच्छा होती है और इसलिए सब कुछ आत्मा की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार चलता है।
इस समस्या को हल करने के लिए हम कह सकते हैं कि जब किसी स्तर विशेष से कोई विधान अभिव्यक्ति में आ जाता है तब तो वह नियत होता है परंतु जहाँ से वह विधान आता है यदि वहीं उसमें उच्चतर चेतना के विधान को प्रभावी किया जाए तो उसमें कुछ भी फेर-बदल किया जा सकता है अन्यथा तो भगवान् की सर्वशक्तिमत्ता का कोई अर्थ ही नहीं था। तब तो यह सारा संसार एक ऐसी सिनेमा की भाँति होता जिसे कि पूर्व में रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब उसका प्रसारण मात्र किया जा रहा है। यदि ऐसा ही होता तब तो यह सारे कर्म के उत्प्रेरण पर ही कुठाराघात करता है और सभी आशा को नष्ट कर देता है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए कोई चीज भले कितनी भी पूर्वनियत क्यों न हो, परंतु सदा ही एक गुह्य संभावना बनी रहती है कि एक उच्चतर चेतना के विधान के द्वारा उसे बदला जा सकता है। स्वयं श्रीअरविन्द व श्रीमाँ वैश्विक विधान को पूरी तरह अतिक्रम करके अतिमानसिक अवतरण की घोषणा करने के लिए, दिव्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए आए थे। इसलिए यदि सब कुछ मानसिक चेतना के वर्तमान स्तर के अनुरूप ही पूर्वनियत होता तब तो इस प्रकार की घोषणाएँ निरर्थक होतीं और दिव्य साम्राज्य की स्थापना एक दिवास्वप्न ही होती। परंतु श्रीमाँ व श्रीअरविन्द कहते हैं कि वे परात्पर के विधान को उतार लाने के लिए आए हैं और उसके द्वारा पृथ्वी पर अज्ञान और मिथ्यात्व के साम्राज्य का अंत करके भागवत् साम्राज्य स्थापित करने आए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर भगवान् की एक ऐसी उपस्थिति विराजमान है जिसके सामने कोई भी विधान लागू नहीं हो सकता। वह स्वतंत्र रूप से अपना विधान बना सकती है और उसे लागू कर सकती है। इसी शक्ति के आधार पर सावित्री ने मृत्यु के देव का सामना करके उसे परास्त कर दिया। इससे हमें यह आशा और आश्वासन प्राप्त होता है कि कोई बड़े से बड़ा विधान भी वास्तव में हमारी आत्मा के लिए बाध्यकारी नहीं होता। इसलिए जब वह दिव्यता हमारे अंदर विराजमान है तब हमें किन्हीं भी विधानों के विषय में कुछ भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु इसे हमें अपने अहं से नहीं समझ लेना चाहिये, जैसा कि प्रायः ही होता है।
अब एक दूसरी चेतना के दृष्टिकोण से देखें तो वास्तव में आप हो परम पुरुष हैं, आप स्वयं ही परम् सत्ता हैं जिसके परे न किसी चीज का कोई अस्तित्व है, और न कोई दूसरी सत्ता है। सारे देवता, सारे ब्रह्माण्ड, सारी सृष्टि सभी कुछ आप ही का अंश है। जब यह चेतना प्रभावी होती है तब तो किसी नियति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी चेतना में तो न केवल स्वतंत्रता ही है, अपितु सब कुछ आप ही की प्रसत्रता के निमित्त होता है। हमारे वेदांत का यही मूल सिद्धांत है कि हम ऐसी किसी चीज के संपर्क में नहीं आ सकते जो स्वयं हमारे अंदर से ही निःसृत न हो। कहने का अर्थ है कि सब कुछ हमारी चेतना की ही उत्पत्ति है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। परंतु यह कोई मानसिक विचार के द्वारा नहीं हो सकता, जब इसका जीवंत अनुभव होता है तभी हमें यह मूलभूत सत्य प्रकट हो सकता है। परंतु यह जगत् प्रपंच इस प्रकार रचा गया है कि इसमें सहज ही व्यक्ति को यह अनुभव नहीं होता। पर इससे इस चेतना की संभावना समाप्त नहीं हो जाती। हम अवश्य ही ऐसी चेतना में जा सकते हैं और स्वयं यह अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार जब हमारी बाहरी प्रकृति तक भी यह अनुभव और यह श्रद्धा प्रभावी हो जाए तब फिर कुछ भी असंभव नहीं है। पांडिचेरी स्थित श्रीअरविन्द आश्रम तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्पष्ट ही है कि वह कोई सामान्य मानवीय रचना नहीं हो सकती। यह तो श्रीमाँ व श्रीअरविन्द के द्वारा अपनी चेतना के बल से एक नये जगत् का सृजन है जहाँ भौतिक जगत् के नहीं अपितु दिव्यतर जगतों के विधान कार्य करते हैं। किसी भी संवेदनशील दृष्टि को यह तुरंत ही स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ भौतिक प्रकृति के नियमों को बदल दिया गया है और केवल भागवत् विधान ही सच्चे रूप से प्रभावी है। किसी न किसी हद तक प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बनाए जगत् में निवास करता है। और जितना ही हम अपने अंदर उस दिव्य तत्त्व के संपर्क में आ जाएँ, उसे अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान कर सकें उतना ही हम प्रभावशाली रूप से एक विशालतर और दिव्यतर जगत् का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हमारे अपने बनाए नियम-विधान प्रभावी होते हैं। इसी कारण महान् व्यक्ति अपने शक्तिशाली प्रभामण्डल का निर्माण कर लेते हैं जिसमें इन्हीं सतही नियमों में उच्चतर विधान को लागू कर वे विलक्षण उपलब्धियाँ और संसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति की तो कल्पना से भी परे होती हैं। श्रीमाताजी के अनुसार श्रीअरविन्द के प्रभामण्डल को तो भौतिक रूप से कुछ मील दूर तक महसूस किया जा सकता था। किस प्रकार श्रीअरविन्द अपने आस-पास के भौतिक वातावरण पर भी पूर्ण नियंत्रण रखते थे इसका उदारहण देते हुए श्री माताजी ने एक घटना बताई। एक बार पाण्डिचेरी में भारी तूफान आया, इसलिए श्रीअरविन्द के कक्ष की खिड़कियाँ आदि बंद करने के लिए जब श्रीमाताक वहाँ गईं तो पाती हैं कि कक्ष के भीतर तो पूर्ण नीरवता थी। बाहर चल रहे भारी तूफान का भीतर कोई प्रभाव तक नहीं था। इस दृष्टांत से साफ हो यह प्रकट होता है कि किस प्रकार आत्मा की शक्ति के द्वारा बाहरी प्रकृति के नियमों को सर्वथा वश में किया जा सकता है, उनमें अभीष्ट फेर-बदल किया जा सकता है।
इसलिए प्रत्येक के लिए यह संभावना खुली है कि वह ऐसी चेतना में प्रवेश कर सकता है, अपने ही एक विशाल और दिव्य जगत् का निर्माण कर सकता है, अपने संकल्प को बाहरी नियमों पर लागू कर सकता है और एक श्रेष्ठतर और दिव्यतर जीवन जी सकता है जो स्वयं उसके लिए और जो कोई उसके संपर्क में आए उसके लिए सार्थक हो।
II. विश्वपुरुष-दर्शन
दोहरा पक्ष
सञ्जय उवाच
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥
३५. सञ्जय ने कहाः केशव के ये वचन सुनकर किरीटी (मुकुटधारी अर्जुन) ने काँपते हुए हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया और अतिशय भय के कारण गद्गद् कंठ से श्रीकृष्ण से (इस प्रकार) कहा।
जब कि इस दर्शन के विकराल रूप का प्रभाव अभी उस पर छाया हुआ है तब भी भगवान् का कथन समाप्त होने के बाद अर्जुन ने जो प्रथम उद्गार प्रकट किये वे मृत्यु की इस मुखाकृति तथा इस संहार के पीछे विद्यमान एक महत्तर उद्धारक तथा आश्वासक सद्वस्तु की एक ओजस्वी व्याख्या करते हैं।
अर्जुन उवाच
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ।। ३६॥
३६. अर्जुन ने कहाः हे हृषीकेश ! यह उचित ही है कि आपके नाम का कीर्तन करने में संसार हर्षित और आनंदित होता है। राक्षस आपसे भयभीत होकर दूर दिशाओं में भाग रहे हैं और समस्त सिद्धों के समुदाय आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं।
इन प्रथम उद्गारों से यह संकेत सामने आता है कि इन भयावह रूपों के पीछे का गूढ़ सत्य एक पुनः आश्वासन देनेवाला प्रोत्साहन और आनंद देनेवाला सत्य है। उसमें ऐसा कुछ है जो जगत् के हृदय को भगवान् के नाम तथा सामीप्य में हर्ष तथा आह्लाद अनुभव कराता है। उस वस्तु का गहन बोध ही हमें काली की घोर आकृति में माँ की मुखछवि के दर्शन कराता है और यहाँ तक कि संहार के बीच में भी प्राणियों के सखा की रक्षक भुजाओं, अनिष्ट या अशुभ के बीच भी एक शुद्ध निर्विकार दयालुता की उपस्थिति तथा मृत्यु के मध्य भी अमृतत्व के स्वामी का अनुभव कराता है।... जिन्हें नष्ट किया जाना है, अशुभ, अज्ञान, निशाचर तथा राक्षसी शक्तियाँ, उन्हें छोड़कर और किसी भी चीज को वास्तव में डरने की आवश्यकता नहीं। उग्रदेव रुद्र की समस्त गतिविधि और क्रिया की प्रवृत्ति लक्ष्य संसिद्धि, दिव्य ज्योति और पूर्णता की ओर होती है।
यह ध्यान देने योग्य बात है कि रुद्र की क्रिया केवल अंधतर चीजों और शक्तियों के प्रति ही होती है, उन चीजों के प्रति जो भागवत् कार्य में, भागवत् अभिव्यक्ति और संसिद्धि में बाधक होती हैं। उनकी क्रिया किसी भी सच्ची चीज के ऊपर नहीं होती। साथ ही जब हमारे भीतर के शत्रुओं पर प्रहार होता है, हमारी गहरी जमी आदतों पर, इच्छाओं-कामनाओं पर सीधे आघात होता है तब अवश्य ही बड़ी मर्मांतक पीड़ा होती है परंतु ऐसे में भीतर से सहायता प्रदान करने के लिए यह आभास भी अवश्य होता है कि भागवत् कृपा के द्वारा ही यह क्रिया हो रही है और इस आभास के सहारे ही व्यक्ति उस पीड़ा को कुछ-कुछ सहन कर पाता है। प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न गठन के अंदर यह आभास भिन्न-भिन्न हो सकता है। कोई इसे अपने आदर्श के रास्ते में आए व्यवधान के रूप में लेकर सहन कर सकता है, कोई इसे भागवत् कृपा की क्रिया के रूप में देख सकता है, कोई इसे दिव्य शक्ति की क्रिया के रूप में देख सकता है जो उसके बंधनों को काटकर उसे ऊर्ध्वमुखी आरोहण पथ पर ले जा रही है। यह क्रिया उसी अनुपात में पीड़ादायक और विकट प्रतीत होती है जिस अनुपात में व्यक्ति अपने निजी सामर्थ्य पर भरोसा जमाए होता है। यदि वह अपने निजी सामर्थ्य की बजाय भागवत् शक्ति के भरोसे रहता है तो भले कितना भी विकट कार्य, कितनी भी भयंकर क्रिया क्यों न हो, व्यक्ति सहज ही उसे स्वीकार कर लेता है और विचलित नहीं होता क्योंकि भागवत् शक्ति के लिए कोई भी चीज विकट नहीं हो सकती।
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रै ।
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ।। ३७ ।।
३७. हे महात्मन् ! वे सब आपको क्यों न नमस्कार करें? क्योंकि आप तो आदि-स्रष्टा और आदि-कर्त्ता हैं और ब्रह्मा से भी अधिक महान् हैं। हे अनंत! हे देवताओं के भी ईश्वर! हे जगत् के आश्रय-स्थान! आप ही अक्षर ब्रह्म, और आप ही सत्-असत् और आप ही जो सत्-असत् से परे है वह परम हैं।
क्योंकि, ये परमात्मा, ये भगवान् केवल बाह्य रूप में ही संहारक हैं, अर्थात् इन सब सीमित रूपों को नष्ट करनेवाले काल हैं : पर अपने-आप में वे अनंत हैं, वैश्व देवताओं के ईश्वर हैं, जिनके अंदर जगत् तथा उसके समस्त कर्म सुदृढ़ रूप से अधिष्ठित हैं.... वे ही सत् और असत् तथा व्यक्त और सदा अव्यक्त का... द्वंद्वात्मक रूप हैं। परन्तु इन सबसे परे जो है वह 'तत्' या 'परम' हैं जो सब परिवर्तनशील वस्तुओं को उस काल की, जिसके लिए सब कुछ सदैव वर्तमान है, अखंड नित्यता में धारण करते हैं। वे अपने अक्षर आत्मा को उस कालातीत नित्यता में धारण करते हैं जिनके काल और सृष्टि नित्य-विस्तारशील रूप हैं।
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्यपरं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।। ३८।।
३८. आप आदि-देव और पुरातन पुरुष हो, आप इस संपूर्ण विश्व के परम विश्रामस्थान हो; आप ज्ञाता और ज्ञेय और परम-पद हो; हे अनंतरूपवाले! आपसे ही यह संपूर्ण विश्व विस्तृत हुआ है।
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्व ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९॥
३९. आप वायु, यम, अग्नि, वरुण और चन्द्रमा हो; आप जीवों के पिता और ब्रह्मा के भी पिता हो; आपको सहस्रों बार नमस्कार है और पुनः आप को बारम्बार नमस्कार है।
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४०॥
४०. हे सर्वात्मन्। आपको सामने से और पीछे से नमस्कार है, आपको सब ओर से ही नमस्कार है; आप अनन्त बलवाले और अनन्त पराक्रम वाले हो, आप सब में व्याप्त और सब कुछ, 'सर्व', हो।
यह पुनः दुहराया गया है कि वे सर्व हैं, वह प्रत्येक और सभी, (सर्वः) हैं। वे अनंत 'विराट' सत् हैं और यहाँ विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति तथा जो कुछ है वह हैं, वे एकमात्र शक्ति तथा सत्ता हैं जो हममें से प्रत्येक के अंदर निहित है....
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ।। ४१।।
४१. आपकी इस महिमा को न जानकर, प्रमाद से अथवा प्रेमवश भी आपको केवल अपना मानव मित्र और साथी समझते हुए मैंने हठपूर्वक जो हे कृष्ण! हे यादव! हे सखा ऐसा जो कुछ भी कहा है;
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ।। ४२ ।।
४२. और हे अच्युत! क्रीड़ा-विहार के अवसर पर, शय्या पर, आसन पर, भोजन के अवसरों पर, अकेले में अथवा सबके साथ में आपका असत्कार किया है उसके लिये मैं, हे अप्रमेय! आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ।
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ।। ४३।।
४३. आप इस संपूर्ण चराचर लोक के पिता हो; आप पूजनीय हो और परम पवित्र आदरणीय हो। हे अतुलनीय बलवाले! तीनों लोकों में कोई भी दूसरा आपके समान नहीं है तब फिर अधिक कैसे हो सकता है?
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडयम्।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ।। ४४।।
४४. इसलिये मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ और अपने शरीर से दण्ड के समान चरणों में प्रणाम करते हुए स्तुति करने योग्य ईश्वर आपसे कृपा के लिये प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे अपने मित्र के और प्रेमी जैसे अपने प्रेमास्पद के अपराधों को सहन करता है इसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन (क्षमा) करें।
अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।
तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। ४५।।
४५. जो पहले कभी नहीं देखा गया था आपके उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ परन्तु मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। हे देवा अपने उस अन्य रूप को ही मुझे दिखलाइये। हे देवों के प्रभो! जगत् के निवासस्थाना प्रसन्न हों।
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ।। ४६।।
४६. मैं आपको पहले के ही समान मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रपाणि रूप में देखना चाहता हूँ। हे सहस्र भुजावाले! हे विश्वरूपधारी! अपने उस चतुर्भुन रूप को ही धारण कीजिये।
[अब] यह विचारधारा... मनुष्य के अन्दर विद्यमान इस एक महान् देव की उपस्थिति की ओर मुड़ जाती है। यहाँ विश्वरूप दर्शन के द्रष्टा की आत्मा को तीन क्रमिक सुझावों के द्वारा समझाया गया है। सर्वप्रथम, उसके अंदर यह बोध हो जाता है कि 'मानव' के इस पुत्र की देह में....मर्त्य मनुष्य की आकृति में सदा ही कोई महान्, निगूढ़ तथा अत्यंत सारयुक्त तत्त्व, परमेश्वर, अवतार, विराट् शक्ति, एकमेव सद्वस्तु, परमोच्च परात्पर पुरुष निहित था। इस गुह्य देवत्व के प्रति, जिसमें मनुष्य तथा उसकी जाति के सुदीर्घ विकास का समस्त मर्म छिपा पड़ा है और जिससे संपूर्ण जगत्-सत्ता अपनी अकथनीय महिमा से युक्त आंतरिक अर्थ प्राप्त करती है, वह अंधा ही रहा था। केवल अब ही वह व्यष्टिभूत ढाँचे में विद्यमान विश्वात्मा को, मानवता के रूप में मूर्तिमंत भगवान् को तथा प्रकृति के इस प्रतीक में परात्पर अंतर्वासी को देखता है।... क्योंकि, वह महान् यथार्थ सत्ता सम तथा अनंत है और व्यष्टि तथा विश्व दोनों में समान ही है। सब से पहले उसे अपना अंधापन, इन भगवान् के प्रति ऐसा व्यवहार कि वे मात्र बाह्य मनुष्य हैं, इनके साथ होनेवाले केवल मानसिक तथा भौतिक संबंध को ही देखना वहाँ उपस्थित महामहिम देव के प्रति एक पाप प्रतीत होता है। क्योंकि, जिन पुरुष को वह कृष्ण, यादव, सखा कहकर पुकारता था ये अपरिमेय-महिमामय, अप्रतिम-प्रभावशाली, सब में अवस्थित एकमेव परमात्मा ही थे जिनकी ये सब प्रजाएँ हैं...।
परंतु दूसरा सुझाव यह है कि मानवीय अभिव्यक्ति तथा मानवीय संबंध के रूप में जो कुछ मूर्तिमंत था वह भी यथार्थता है जो विराट्पुरुषदर्शन के भयंकर स्वरूप के साथ रहती है तथा उसकी भयंकरता को हमारे मन के लिए कम कर देती है। विश्वातीत तथा वैश्व पहलुओं को भी देखना होगा, क्योंकि ऐसे साक्षात्कार के बिना मानवता की सीमाओं को पार नहीं किया जा सकता। उस एकीकारक एकत्व में सब कुछ को समाविष्ट करना होगा। परंतु केवल अपने-आप में वह एकत्व विश्वातीत आत्मा और अपरा प्रकृति के अंदर बद्ध और घिरी हुई इस अंतरात्मा के बीच बड़ी भारी खाई बना देगा। अपने पूर्ण वैभव में अनंत उपस्थिति या सत्ता सीमित, व्यष्टिरूप तथा प्रकृतिगत मनुष्य की पृथक् क्षुद्रता के लिए अतीव अभिभूतकारी या विह्वल करने वाली होगी। एक ऐसी संयोजक कड़ी की आवश्यकता है जिसके द्वारा वह इन विराट् परमेश्वर को अपनी वैयक्तिक एवं प्राकृतिक सत्ता में, अपने समीप स्थित देख सके, केवल सर्वशक्तिमान् रूप में ही नहीं जो विश्वव्यापी अपरिमेय शक्ति के द्वारा उसकी संपूर्ण सत्ता को नियंत्रित करते हैं अपितु एक घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध के द्वारा उसे आश्रय देने तथा एकत्व की ओर उठा ले जाने के लिए मानव-रूप में भी मूर्तिमंत हैं। जिस पूजा-भक्ति के द्वारा सीमित प्राणी अनंत के सामने नमन करता है वह उस समय अपना समस्त माधुर्य प्राप्त कर लेती है तथा सख्य और एकत्व के घनिष्ठतम सत्य के निकट पहुँच जाती है जब वह गहन होकर उस अधिक घनिष्ठ उपासना का रूप धारण कर लेती है जो ईश्वर के पितृभाव एवं सख्य-भाव में तथा परमात्मा और हमारी मानव आत्मा एवं प्रकृति के बीच होनेवाले आकर्षक प्रेम के भाव में निवास करती है। क्योंकि, भगवान् मानव-आत्मा और देह में वास करते हैं; वे मानव-मन तथा आकार को अपने चारों ओर खोलकर वस्त्र की भाँति धारण करते हैं। वे उन मानवीय संबंधों को ग्रहण करते हैं जिन्हें आत्मा मर्त्य शरीर में स्थापित करती है और वे संबंध ईश्वर में अपना निजी पूर्णतम अर्थ एवं महत्तम अनुभूति और चरितार्थता प्राप्त करते हैं। यह वैष्णव भक्ति है जिसका बीज यहाँ गीता के शब्दों में निहित है पर जिसने आगे चलकर अधिक गंभीर, उल्लासमय और अर्थपूर्ण विस्तार प्राप्त कर लिया है।
और इस दूसरे सुझाव से तुरंत ही एक तीसरा सुझाव उत्पन्न होता है। विश्वातीत और विश्वव्यापी पुरुष का रूप मुक्त आत्मा की सामर्थ्य के लिए एक महान्, उत्साहप्रद तथा शक्तिदायक रूप है, शक्ति का स्रोत है, सम तथा उदात्त करनेवाला और सबका औचित्य सिद्ध करनेवाला दिव्य दर्शन है; परंतु सामान्य मनुष्य के लिए यह विह्वल कर देने वाला, भयावह तथा अग्राह्य है। और जो सत्य आश्वासन या निर्भयता प्रदान करता है, उसका ज्ञान होने पर भी, सर्वसंहारक काल के भीषण तथा शक्तिशाली रूप के और अगम्य संकल्प तथा विस्तृत अथाह गहन क्रिया के पीछे, कठिनाई से ही समझ में आता है। किन्तु दिव्य नारायण का एक मध्यस्थता करनेवाला कृपापूर्ण रूप भी है, उन नारायण का जो मनुष्य के इतने निकट तथा उसके अंदर विद्यमान ईश्वर हैं, युद्ध और यात्रा के सारथी हैं, सहायक-शक्ति की चार भुजाओं से युक्त हैं, परमेश्वर के मानवीय प्रतीक हैं, असंख्यों भुजाओं युक्त ये विराट् पुरुष नहीं। इस मध्यस्थता करने वाले रूप को ही हमें नित्य-निरंतर अपने अवलंब के रूप में अपने सम्मुख रखना होगा। क्योंकि, भगवान् का यह नारायण-रूप ही आश्वासनदायी या निर्भयकारी सत्य का प्रतीक है।
अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर अपना सामान्य नारायण-रूप, 'स्वकं रूपम्' प्रसाद, प्रेम, माधुर्य और सौंदर्य से संपन्न अभीष्ट रूप पुनः धारण करते हैं, परंतु, उससे पहले वे उस दूसरे शक्तिशाली विराट् रूप की, जिसे वे छिपानेवाले ही हैं, अमित महिमा उद्घोषित करते हैं।
यदि यह विश्वरूपदर्शन प्राप्त न हो तो परमात्मा के बारे में हमारी धारणाएँ, उनके विषय में हमारे सीमित मानसिक दृष्टिकोण टूटते नहीं। मानसिक रूप से हम कितने भी उदात्त चित्रण या परिकल्पनाएँ कर लें कि परमात्मा असीम हैं, विशाल हैं, आदि-आदि परंतु इन सब से परमात्मा के विषय में हमारा मानसिक दायरा बहुत ही सीमित और संकुचित बना रहता है और बिना वह साक्षात्कार हुए हम इस पूर्ण भगवत्ता के दर्शन नहीं कर सकते। संभव है कि व्यक्ति को किन्हीं देवताओं आदि के अनुभव या दर्शन प्राप्त हो चुके हों, परंतु एक समग्र भगवत्ता का दर्शन एक सर्वथा भिन्न चीज है। इस दर्शन में भगवान् के व्यष्टिगत, वैश्विक और परात्पर, सभी रूपों का समग्रता में दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब अर्जुन को अपनी सीमितता का भान होता है तब वह भगवान् से प्रार्थना करता है कि उसे उनका वह सच्चा रूप दिखाया जाए। केवल उनकी कृपा से ही वह दर्शन प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं।
दूसरे, यदि मनुष्य के अंदर अपनी सीमितता से निकलकर भगवान् के उस विराट् रूप को देखने का कोई उपाय न होता तब तो व्यक्ति उनके उस रूप को देखकर भयभीत ही होता। इसी दूरी को कम करने के लिए, एक संयोजक कड़ी प्रदान करने के लिए परमात्मा मनुष्य के साथ सभी प्रकार के संबंधों के मार्ग खोल देते हैं। और जिस भी भाव से व्यक्ति उनके पास जाता है वे उसी रूप में उसके साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। कोई उन्हें अपने मालिक के रूप में मानता है तो कोई पुत्र के रूप में, कोई मित्र के रूप में मानता है तो अन्य दूसरा किसी अन्य रूप में। इस प्रकार भगवान् ने संपर्क और संबंध साधने के अनेकानेक मार्ग खोल दिये हैं जिनके द्वारा मनुष्य उनके पास पहुँच सकता है, उनसे संबंध स्थापित कर सकता है। उन संबंधों के माध्यम से हमें परमात्मा का कम या अधिक आभास प्राप्त होता है क्योंकि वास्तव में तो यह परमात्म सत्ता हमारे स्वयं के अंदर ही अंतर्निहित है। इसीलिए हम इन सब संबंधों के माध्यम से उनके संपर्क में आ सकते हैं। और जब वह दर्शन प्राप्त होता है तब वह उन संबंधों की सभी सीमितताएँ नष्ट कर देता है। और चूंकि वह तत्त्व हमारे अपने अंदर भी निहित होता है इसलिए हम उसे सहन भी कर पाते हैं अन्यथा तो उस विराट् रूप को सहन नहीं कर सकते थे।
तीसरे, विरारूप के वर्णन में ही भगवान् चतुर्भुज रूप से अपने नारायण रूप को धारण करते हैं। प्रतीकरूप में चार हाथ भगवान् के अनेकविध रूप से सहायता करने के स्वभाव को दर्शाते हैं। भगवान् का यह सहायक रूप तो जो कोई भी उनकी ओर मुड़ता है उसे पहले ही महसूस हो जाता है कि किस प्रकार समय-समय पर भगवान् सहायता करते हैं। और इसी की सहायता से व्यक्ति भगवान् के साथ संबंध स्थापित करता है। जब व्यक्ति भगवान् से कोई प्रार्थना करता है, उनसे कुछ माँग करता है और जब वह पूर्ण हो जाती है तब उसे उनकी सत्ता में विश्वास हो जाता है और इस प्रकार धीरे-धीरे उसका उनसे संबंध स्थापित हो जाता है। अतः नारायण के रूप में यह परमात्मा का सहायक स्वरूप है।
श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ।। ४७।।
४७. श्रीभगवान् ने कहा : हे अर्जुन! मेरे अनुग्रह से जो तू अब देख रहा है वह मेरा परम रूप है, मेरा ज्योतिर्मय शक्तिवाला, विश्वात्मक, आदि, अनन्त रूप है जिसे मनुष्यों में तेरे अतिरिक्त अन्य किसी ने आज तक नहीं देखा है। यह मैंने अपने आत्म-योग से तुझे दिखाया है।
क्योंकि, यह स्वयं मेरी आत्मा एवं अध्यात्मसत्तामात्र का रूप है, यह लौकिक जीवन में निजशक्ति से मूर्तिमान् हुए साक्षात् पुरुषोत्तम ही हैं और मेरे साथ पूर्ण रूप से योगयुक्त जीव इसे स्नायविक अंगों के किसी प्रकार के कंपन या मन के किसी भी भ्रम एवं भ्रांति के बिना देखता है, क्योंकि वह इसकी बाह्य आकृति में विद्यमान भीषण तथा विह्वल कर देनेवाले तत्त्व का ही नहीं अपितु इसके उच्च तथा अभयप्रद अर्थ को भी जानता है।
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुयैः ।
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।। ४८।।
४८. हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुना न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान-उपकारों से या क्रिया-अनुष्ठानों से या कठोर तपों से मेरा यह रूप इस लोक में तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है।
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् ।
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।। ४९।।
४९. मेरे इस भयानक रूप को देखकर तू भयभीत न हो और तू संभ्रमित न हो। भय को दूर हटाकर प्रसन्नचित्त होकर मेरे इस दूसरे रूप को तू फिर देख।
सञ्जय उवाच
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ।। ५० ।।
५०. सञ्जय ने कहाः अर्जुन को ऐसा कहकर वासुदेव ने पुनः अपने नारायण रूप को प्रकट किया; अपने सौम्य अथवा कृपा रूप को धारण करके महात्मन् कृष्ण ने भयभीत हुए अर्जुन को सान्त्वना दी।
अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ।। ५१।।
५१. अर्जुन ने कहाः हे जनार्दन! आपके इस सौम्य मानव रूप को पुनः देखकर अब मैं स्वस्थचित्त, शान्तचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ।
श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ।। ५२ ।।
५२. श्रीभगवान् ने कहाः मेरे जिस महान् रूप को तूने देखा है इसका देखा जाना अत्यंत कठिन है; यहाँ तक कि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा करते रहते हैं।
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ।। ५३॥
५३. जिस रूप में मुझे तूने देखा है उस रूप में मुझे न वेदों के अध्ययन से, न तप के द्वारा, न दान से और न यज्ञों के द्वारा देखा जा सकता है।
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ।। ५४।।
५४. हे परन्तप! उस भक्ति से जो सभी कुछ में केवल मुझे स्वीकार करती है, मेरी आराधना करती है और मुझसे प्रेम करती है, केवल उसी के द्वारा मैं इस रूप में देखा और जाना जा सकता हूँ और यहाँ तक कि प्रवेश भी किया जा सकता हूँ।
तब भला इस विराट् रूप की वह विलक्षणता क्या है जिसके कारण यह संज्ञान से या पहचान पाने से इतना ऊपर उठा हुआ है कि मानव-ज्ञान का संपूर्ण सामान्य प्रयास और यहाँ तक कि उसके आध्यात्मिक पुरुषार्थ का अंतरतम तप भी, बिना सहायता के, इसके दर्शन लाभ करने के लिये पर्याप्त नहीं है? वह यह है कि अन्य साधनों से मनुष्य एकमेव सत् के इस या उस ऐकांतिक पक्ष को ही, उस 'एकं सत्' के व्यक्तिगत, विश्वगत या विश्वातीत रूपों या पक्षों को ही जान सकता है, पर भगवान् के समस्त रूपों के इस महत्तम समन्वयकारी एकत्व को नहीं जान सकता जिसमें एक ही साथ और एक ही दर्शन में सब कुछ अभिव्यक्त, अतिक्रांत और संसिद्ध रहता है। क्योंकि यहाँ विश्वातीत, विश्वव्यापी और व्यक्तिगत ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, अनंत और सीमित, देश, काल और कालातीतता, सत्ता और संभूति, जो कुछ भी हम परमेश्वर के बारे में सोचने का यत्न कर सकते हैं तथा जो कुछ उनके बारे में जानते हैं वह सब, फिर चाहे वह निरपेक्ष सत्ता के विषय में हो या व्यक्त सत्ता के, एक अनिर्वचनीय एकत्व में अद्भुत ढंग से प्रकाशित हो जाता है। यह दर्शन केवल अनन्य भक्ति एवं प्रेम तथा उस घनिष्ठ एकता के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं जो कर्म और ज्ञान की पूर्णता का सर्वोच्च शिखर होती है। तब पुरुषोत्तम के इस परमोच्च रूप को जानना तथा देखना और इसमें प्रवेश करना तथा इसके साथ एकमय होना संभव हो जाता है, और गीता अपने योग का यही लक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत करती है। एक परम चेतना है जिसके द्वारा परात्पर की महिमा में प्रवेश करना तथा उनके अंदर अक्षर आत्मा और समस्त क्षर भाव को धारण करना संभव है, - सबके साथ एकीभूत और फिर भी सबसे ऊपर होना, जगत् को अतिक्रांत कर जाना और फिर भी विश्वगत ईश्वर तथा विश्वातीत ईश्वर दोनों की संपूर्ण प्रकृति का एक साथ आलिंगन करना संभव है। निश्चय ही अपने मन और शरीर की कैद में बद्ध सीमित मनुष्य के लिए ऐसा करना कठिन है: किंतु, भगवान् कहते हैं...
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।। ५५।।
______________________________
* सभी जीव उस परम सत्ता के द्वारा अस्तित्वमान हैं; सभी पदार्थ ईश्वर की आकृतियाँ हैं; समस्त विचार, कर्म, भाव और प्रेम उन्हीं से उद्भूत होते हैं और उन्हीं में लौट जाते हैं, उनके सभी परिणामों के वे ही उद्गम, आश्रय और गुप्त लक्ष्य हैं। इन्हीं देवाधिदेव, इन्हीं परम सत्ता के प्रति पूर्णयोग की भक्ति उँड़ेली जाएगी और ऊपर उठेगी। परात्पर रूप में यह उन्हें पूर्ण ऐक्य के हर्षावेश में ढूँढ़ेगी; अपने विश्वमय रूप में यह उन्हें गुणों और सभी रूपों और सर्वभूतों में विश्वव्यापी आनन्द और प्रेम के साथ ढूँढ़ेगी, अपने वैयक्तिक रूप में यह उनके साथ वे सभी मानवीय सम्बन्ध स्थापित करेगी जिन्हें प्रेम व्यक्ति व व्यक्ति के बीच उत्पन्न करता है।
...मनन और दर्शन करना, सभी वस्तुओं में अनवरत उन्हीं का चिन्तन और सदा-सर्वदा और सर्वत्र उन्हीं के दर्शन करना इस भक्तिमार्ग का अनिवार्य अंग है। जब हम भौतिक प्रकृति के पदार्थों पर दृष्टिपात करें तो उनके अन्दर हमें अपने दिव्य प्रियतम को देखना होगा; जब हम मनुष्यों और जीवों को देखें तो उनके अन्दर हमें उन्हीं को देखना होगा और उनके साथ अपने सम्बन्ध में हमें यह देखना होगा कि हम उन्हीं के आकारों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं; जब जड़ जगत् की सीमा लाँघकर हम अन्य स्तरों की सत्ताओं का ज्ञान लाभ करें या उनसे सम्बन्ध स्थापित करें तब भी हमें यही विचार अथवा दृष्टि अपने मनों के प्रति प्रत्यक्ष बनानी होगी।... सभी देवताओं में हमें इन्हीं एक ईश्वर को देखना होगा जिन्हें हम अपने हृदय और अपनी सम्पूर्ण सत्ता से पूजते हैं; वे उन्हीं के देवत्व के आकार हैं। अपने आध्यात्मिक आलिंगन को इस प्रकार विस्तारित करते हुए हम एक ऐसे बिन्दु पर जा पहुँचते हैं जहाँ सब कुछ वही होते हैं और इस चेतना का आनन्द हमारे लिये संसार को देखने का हमारा सामान्य अटूट ढंग बन जाता है।
५५. हे पाण्डव! जो मनुष्य मेरे कार्य करता है और मुझे ही परम लक्ष्य स्वीकार करता है, मेरी भक्ति करता है, आसक्ति से मुक्त है, समस्त भूतों के प्रति वैरभाव से रहित है वह मनुष्य मुझे प्राप्त होता है।
दूसरे शब्दों में, निम्न प्रकृति से ऊपर उठना, समस्त प्राणियों से एकता, विश्वव्यापी ईश्वर तथा परात्पर भाव के साथ एकत्व, कर्मों में हमारी इच्छा का भगवान् की इच्छा के साथ एकत्व, एकमेव के लिए तथा सब में स्थित ईश्वर के लिए परम प्रेम, - यही उस चरम-परम आध्यात्मिक आत्म-अतिक्रमण तथा उस अकल्पनीय रूपांतर का मार्ग है।
----------------------------------------
• जो आत्मा अपने-आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को दे देती है, उसे ईश्वर भी अपने-आप को पूर्ण रूप से दे देते हैं। केवल वही जो अपनी सम्पूर्ण प्रकृति को अर्पित कर देता है, आत्मा को प्राप्त करता है। केवल वही जो सब कुछ दे सकता है, सर्वत्र विश्वमय भगवान् का रसास्वादन कर सकता है। केवल एक परम् आत्मोत्सर्ग ही परम् को प्राप्त करता है। हम जो कुछ भी हैं उस सब को यज्ञ द्वारा ऊपर उठा ले जाने से ही हम सर्वोच्च देव को साकार रूप में प्रकट करने और यहाँ परात्पर आत्मा की अन्तर्यामी चेतना में निवास करने में समर्थ हो सकते हैं... उस एकमेव देव के प्रति, जो एक साथ ही हमारी अन्तर्यामी आत्मा एवं चारों ओर से परिवेष्टित करने वाला सर्वं है, तथा इस या अन्य किसी भी अभिव्यक्ति से परे परम् सद्वस्तु है, और गुप्त रूप से एक साथ ये सभी चीजें है, जो सर्वत्र निगूढ़ अन्तर्यामी परात्परता है।
प्रश्न : भक्ति कृपासाध्य है या पुरुषार्थसाध्य है?
उत्तर : वास्तव में इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस ओर पुरुषार्थ भी हम भगवान् की कृपा के बिना नहीं कर सकते। कृपा का अपना ही एक विधान होता है। और सच कहें तो पार्थिव जगत् में अंध-शक्तियों का जिस प्रकार का आतंक है उसमें एक कदम भी सकुशल चल पाना असीम कृपा का ही परिणाम है अन्यथा विरोधी शक्तियाँ तो जीवन को ही समूल नष्ट कर देना चाहती हैं ताकि किसी प्रकार का कोई ऊर्ध्वमुखी आरोहण हो ही न पाए। इसलिए हम कभी भी इस बात का पूरा अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि किस हद तक कृपा हमारे लिये कार्य कर रही है। यह तो हुई कृपा और पुरुषार्थ की बात।
अब, यदि हमारे मन में भगवान् के दर्शन की माँग उठती है तो हम दर्शन के उतने अधिकारी नहीं रहते। ज्यों ही किसी प्रकार की कोई माँग उठती है वह हमें अनधिकारी बना देती है क्योंकि सच्ची भक्ति में किसी प्रकार की कोई माँग नहीं होती। अठारहवें अध्याय में इसे अधिक स्पष्ट रूप से निरूपित किया जाएगा। सामान्यतः व्यक्ति यही समझेगा कि जब पूर्ण भक्ति के प्रभाव से अर्जुन को विरारूप के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं तो फिर आगे शेष क्या रह जाता है। परंतु ज्यों-ज्यों गीता अपने विकासक्रम में आगे बढ़ती है त्यों ही त्यों अधिकाधिक गूढ़ तत्त्वों और रहस्यों को उद्घाटित करती जाती है।
इस प्रकार ग्यारहवाँ अध्याय 'विश्वरूपदर्शनयोग' समाप्त होता है।
बारहवाँ अध्याय
मार्ग और भक्त
गीता के ग्यारहवें अध्याय में उसकी शिक्षा का मूल उद्देश्य संसिद्ध किया जा चुका है और किसी सीमा तक उसे पूर्णता तक भी लाया गया है। जगत् के लिए तथा उन परमात्मा के साथ एक होकर, जो इस जगत् में और इसके सब प्राणियों में निवास करते हैं तथा जिनके अंदर इस जगत् का समस्त कार्य-व्यवहार होता है, दिव्य कर्म करने का आदेश दिया जा चुका है और विभूति द्वारा उसे स्वीकार भी किया जा चुका है। शिष्य को उसके सामान्य मनुष्य के पुराने भाव से, उसके अज्ञान के मापदंडों, प्रेरक-भावों, दृष्टिकोण तथा अहंकारमय चेतना से तथा उस सबसे दूर हटा लिया गया है जिसने उसके आध्यात्मिक संकटकाल में अंततः उसका साथ छोड़ दिया था। ठीक वही कार्य जिसे उस पूर्व आधार पर उसने त्याग दिया था, वही घोर कर्म, वही भयानक संघर्ष अब एक नये आंतरिक आधार पर उसे स्वीकार तथा ग्रहण करा दिया गया है।.... परंतु इस महान् आध्यात्मिक परिवर्तन के संपूर्ण अर्थ को प्रकाशित करने के लिए अभी कुछ और भी कहना बाकी है। बारहवाँ अध्याय इस शेष बचे ज्ञान की ओर ले जाता है और उसके बाद के अंतिम छः अध्याय इसे एक महान् और चरम निष्कर्ष तक विकसित कर देते हैं। यह बात, जिसे कहना अभी बाकी है, आध्यात्मिक मोक्ष के संबंध में वर्तमान वेदांतिक विचार तथा उस विशालतर सर्वग्राही स्वतंत्रता के पारस्परिक भेद पर अवलंबित है जिसे गीता की शिक्षा आत्मा के सम्मुख खोल देती है। अब गीता सीधे उस भेद की ओर मुड़ती है।
यहाँ जिस विषय को गीता सर्वप्रथम स्पष्ट करेगी वह भगवान् की ओर जाने वाले दो मार्गों के विषय में है। एक मार्ग है पारंपरिक साधना आदि का मार्ग, योगी-तपस्वियों तथा ज्ञानियों का मार्ग जिसमें व्यक्ति को निज सामर्थ्य के आधार पर, किन्हीं साधना पद्धतियों का कठोरतापूर्वक पालन करते हुए चलना होता है जिसमें व्यक्ति जंगल में जाकर ध्यान आदि करता है, समाधि लगाता है, और दूसरा मार्ग है भगवान् की भक्ति का मार्ग जिसमें सारे कर्म भगवान् के निमित्त किये जाते हैं। इन दोनों ही मार्गों में श्रेष्ठ कौनसा है? इस विषय में गीता का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट और निर्णायक है। गीता भक्ति को ही निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ बताती है। हालाँकि ज्ञान, तपस्या आदि के मार्ग भी भगवान् की ओर ही ले जाते हैं परंतु उनका अभ्यास बहुत दुष्कर भी है और साथ ही उनसे जो फल प्राप्त होता है वह भक्ति से प्राप्त होने वाले फल की तुलना में निम्नतर भी है। भक्ति का मार्ग सीधे ही भगवान् की ओर ले जाता है और अन्य मार्गों से अधिक फलप्रद भी है।
गीता का मोक्ष एकमेव के भीतर होनेवाले लय में आत्मा की वैयक्तिक सत्ता का आत्म-विस्मृतिपूर्ण विलोए नहीं है, 'सायुज्य मुक्ति' नहीं है; वह एक साथ ही सब प्रकार का मिलन है।... परंपरागत ज्ञानयोग का लक्ष्य एकमेव अनंत सत् में अगाध लय अर्थात् 'सायुज्य' है; वह केवल उसी को संपूर्ण मोक्ष मानता है। भक्तियोग शाश्वत रूप से उसी में निवास या उससे निकटता, 'सालोक्य, सामीप्य', को ही महत्तर मोक्ष मानता है। कर्मयोग सत्ता तथा प्रकृति की शक्ति में एकत्व, 'सादृश्य', की ओर ले जाता है : परंतु गीता अपनी उदार समग्रता में इन सबको समा लेती है और सभी को एक महत्तम एवं समृद्धतम दिव्य स्वतंत्रता तथा पूर्णता में एकीभूत कर देती है...
यह स्मरण रखना होगा कि निर्गुण अक्षर पुरुष तथा उन परमात्मा के बीच विभेद जो एक साथ निर्वैयक्तिक सत् भी हैं और दिव्य व्यक्ति भी और इन दोनों से अधिक भी बहुत कुछ हैं, - यह महत्त्वपूर्ण विभेद, जो बाद के अध्यायों में तथा उस दिव्य "अहम्" में सूचित किया गया है जिसका श्रीकृष्ण अहम्, माम् शब्दों द्वारा बारम्बार उल्लेख कर चुके हैं, अभी तक सर्वथा स्पष्ट और सुनिश्चित रूप में नहीं बतलाया गया है।...इस भेद के विषय में अर्जुन से ही प्रश्न करवाया जाता है।
अर्जुन उवाच
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ।। १।।
१. अर्जुन ने कहाः इस प्रकार निरंतर युक्त रहते हुए जो भक्त आपको खोजते हैं और जो अव्यक्त अक्षरब्रह्म को खोजते हैं, इनमें से किन्हें योग का महत्तर ज्ञान है?
सार-रूप में वह यह कहता है कि आप सभी भूतों के परम मूल और उद्गम हैं, सब वस्तुओं के भीतर अंतर्यामी उपस्थिति हैं, अपने रूपों के द्वारा विश्व में व्याप्त शक्ति हैं, एक ऐसे 'व्यक्ति' हैं जो अपनी विभूतियों में, प्राणियों में, तथा प्रकृति में अभिव्यक्त हैं और अपने महान् विश्व-योग के द्वारा जगत् में तथा हमारे हृदयों में कर्मों के अधीश्वर के रूप में विराजमान हैं। इस रूप में मुझे अपनी सारी सत्ता, चेतना, विचारों, भावनाओं और कार्यों में आपको जानना, पूजना और अपने-आपको आपके साथ युक्त 'सतत-युक्त' करना है। पर तब इन अक्षर का क्या होगा जो कभी व्यक्त नहीं होते, कभी कोई रूप धारण नहीं करते, समस्त कर्म से दूर तथा उससे पृथक् रहते हैं, जगत् के साथ अथवा इसकी किसी भी वस्तु के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्च स्थापित नहीं करते, नित्य शांत, एक, निर्गुण और अचल बने रहते हैं? सभी प्रचलित मतों के अनुसार यह शाश्वत आत्मा महत्तर तत्त्व है और अभिव्यक्तिगत परमेश्वर एक कनिष्ठतर रूप हैः 'अव्यक्त' ही शाश्वत आत्मा हैं, 'व्यक्त' नहीं। तब भला जो योग अभिव्यक्ति को स्वीकार करता है, एक हीनतर वस्तु को अंगीकार करता है, वह फिर भी एक अधिक महान् योग-ज्ञान कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का श्रीकृष्ण जोरदार निर्णायकता के साथ उत्तर देते हैं।
श्रीभगवान् उवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ।। २।।
२. श्रीभगवान् ने कहाः जो लोग अपने मन को मुझमें प्रतिष्ठित करते हैं और परम श्रद्धा से युक्त, निरंतर मेरे साथ युक्त रहते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं सर्वाधिक पूर्णता से योग में युक्त मानता हूँ।
परम श्रद्धा वह है जो सबके अन्दर ईश्वर को देखती है और उसकी दृष्टि में अभिव्यक्ति तथा अनभिव्यक्ति एक ही परमेश्वर हैं। पूर्ण युक्तभाव वह है जो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कर्म में तथा संपूर्ण प्रकृति में भगवान् से भेंट करता है। परन्तु परमेश्वर कहते हैं कि जो एक दुष्कर आरोहण के द्वारा अनिर्देश्य अव्यक्त अक्षर की ही खोज करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि, वे अपने लक्ष्य में गलत नहीं हैं, परन्तु वे एक अधिक कठिन तथा कम पूर्ण और कम सिद्ध मार्ग का अनुसरण करते हैं।
अतः यहाँ बड़े ही निर्णायक रूप में भगवान् ने उपासना करने वाले भक्त की श्रेष्ठता घोषित कर दी है। भले ही अनिर्देश्य अक्षर की खोज का मार्ग किन्हीं को बहुत ही गंभीर साधनामय मार्ग प्रतीत होता हो और भक्तिमार्ग कम गंभीर और अपरिपक्व प्रकृति वाले लोगों का मार्ग प्रतीत होता हो तब भी सच्चाई यह है कि अक्षर की प्राप्ति का मार्ग दुष्कर होने के कारण ही कोई अधिक फलदायक नहीं बन जाता। यह मार्ग अधिक
दुष्कर भी है और भक्तिमार्ग की अपेक्षा कम पूर्ण और कम सिद्ध मार्ग है। साथ ही, केवल उन्हें छोड़ कर जिनकी प्रकृति बनी hat 5 अक्षर की खोज के अनुकूल है, सामान्य मनुष्य के लिए तो भक्ति मार्ग hat BT अधिक सुगम है जबकि दूसरा मार्ग उनके लिए अप्राकृतिक है। इसीलिए भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है।
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ।। ३ ।।
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।। ४।।
३-४. और जो लोग अपनी समस्त इन्द्रियों को संयत करके, सर्वत्र समदृष्टि होकर, समस्त प्राणियों के कल्याण के भाव से भावित होकर अक्षर, अनिर्देश्य (अनिर्वचनीय), अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल और नित्य या ध्रुव की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्रास होते हैं।
निषेधात्मक निष्क्रियता, मौन-वृत्ति, जीवन और कर्म के संन्यास की पद्धति को, जिसके द्वारा लोग अनिर्देश्य परम की खोज करते हैं, गीता की दर्शनप्रणाली में स्वीकृत और समर्थित किया गया है, पर केवल एक गौण रिआयती अनुमोदन के रूप में। यह निषेधात्मक ज्ञान सनातन ब्रह्म की ओर सत्य के केवल एक पक्ष' को लेकर चलता है और वह पक्ष है जहाँ, 'दुःखं देहवद्भिरवाप्यते', प्रकृतिस्थ देहधारी जीवों के लिए पहुँचना अत्यंत कठिन है; यह पद्धति बड़े ही खास तरीके के और यहाँ तक कि एक अनावश्यक रूप से दुर्गम मार्ग से अग्रसर होती है जिस पर चलना 'छुरे की धार पर चलने के समान कष्टप्रद और दुष्कर' है।
उस मार्ग के सरलतम रूप में, उन्हें अव्यक्त कूटस्थ तक पहुँचने के लिए यहाँ विद्यमान अभिव्यक्त अक्षर के द्वारा ही आरोहण करना होता है। यह अभिव्यक्त अक्षर मेरी ही अपनी सर्वव्यापक निर्वैयक्तिकता और नीरवता है: यह बृहत्, अचिंत्य, ध्रुव, अचल, सर्वव्यापक स्वरूप वाला होकर व्यक्तित्व को क्रिया को आश्रय प्रदान करता है पर उसमें भाग नहीं लेता। यह मन की पकड़ में नहीं आता; इसे केवल निश्चल आध्यात्मिक निर्वैयक्तिकता और नीरवता के द्वारा ही उपलब्ध किया जा सकता है और जो लोग केवल इसी का अनुसंधान करते हैं उन्हें मन तथा इंद्रियों के व्यापार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना और यहाँ तक कि उसे सर्वथा अपने अन्दर समेट लेना होता है। परन्तु फिर भी अपनी बुद्धि की समता के कारण और सब पदार्थों में एक ही आत्मा को देखने तथा सर्वभूतों के हित में रत नीरव चित्त की शांत दयालुता के कारण वे भी सब पदार्थों तथा प्राणियों में मुझसे ही मिलते हैं। जो लोग सर्वभावेन भगवान् के साथ युक्त होते हैं, और जगत् के पदार्थों के अचिंत्य जीवंत स्रोत, 'दिव्यं पुरुषमचिन्त्यरूपम्', में व्यापक और पूर्ण रूप से प्रवेश करते हैं, उनके समान ही, इस कठिनतर ऐकांतिक एकत्व के द्वारा संबंधातीत अव्यक्त कूटस्थ की ओर आरोहण करनेवाले ये जिज्ञासु भी अंत में उसी सनातन को प्राप्त करते हैं। परन्तु यह कम सीधा तथा अधिक दुर्गम मार्ग है; यह आध्यात्मीकृत मानव प्रकृति की पूर्ण और स्वाभाविक गति नहीं है।
इस मार्ग में हमारी सभी सहज सामान्य वृत्तियों का बड़े भारी संकल्प के द्वारा निषेध करना होता है और उनका कठोर रूप से निग्रह कर के उन पर नियंत्रण लागू किया जाता है। परंतु थोड़ी सी चूक से भी व्यक्ति की सारी मेहनत निरर्थक हो जाती है और व्यक्ति अपनी अवस्था से नीचे गिर जाता है जहाँ से उसे पुनः अधिक मेहनत के साथ आरंभ करना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मानव प्रकृति के लिए स्वाभाविक नहीं है अपितु मनुष्य की प्रकृति का बलात् नियंत्रण कर के उस पर आरोपित
किया गया अनुशासन है। इस कारण यह पूरी पद्धति मानव प्रकृति के लिए कष्टकर और दुष्कर होती है और ऐसी होते हुए भी परिणाम में यह भक्तिमार्ग से कम फलप्रद है। इसलिए किसी प्रकृति विशेष के लिए तो यह मार्ग उचित हो सकता है परंतु सर्वसामान्य के लिए तो भक्ति मार्ग ही अधिक सुगम होता है।
____________________________
* हर एक, व्यक्तिगत तौर पर, अपने 'मूल उद्गम' और अपनी सत्ता के चरम तक पहुँच सकता है; उसका मूल उद्गम और उसकी सत्ता का चरम रूप 'शाश्वत', 'अनंत' और 'परम' से अभिन्न है। इसलिये, यदि तुम इस मूल तक पहुँच जाते हो, तो तुम 'परम' तक पहुँच जाते हो। किन्तु तुम वहाँ एक रेखाकार गति में जाते हो (मेरे शब्दों को हूबहू वर्णन के रूप में न लो, समझे, यह तो केवल अपनी बात को समझाने के लिये है)। यह एक रेखाकार उपलब्धि है जो एक बिन्दु पर समाप्त हो जाती है, और यह बिन्दु 'परम् पुरुष' से संयुक्त होता है - जो तुम्हारी उच्चतम संभावना है। दूसरे मार्ग से ऐसी सिद्धि होती है जिसे गोलाकार कह सकते हैं, क्योंकि यह शब्द ही सबसे अच्छे ढंग से किसी ऐसी चीज का भाव देता है जो सबको समाये हुए हो, और इससे जो सिद्धि प्राप्त होती है वह कोई एक बिन्दु तक ही नहीं रहती अपितु एक संपूर्णता होती है जिसमें से कोई चीज बाकी नहीं छूटती ...
....एक बूँद जल के साथ पूर्ण तादात्म्य द्वारा तुम समुद्र को उसके तत्त्व में जान सकते हो, और दूसरे तरीके से तुम समुद्र को केवल तत्त्व में नहीं अपितु उसकी संपूर्णता में जान सकते हो... यह कहा जा सकता है कि जब तुम केवल अपने निजी सामर्थ्य पर निर्भर होते हो, तो व्यक्ति-भाव अपनाने वाली हर चीज अपने अंदर व्यक्तित्व के गुण को और साथ ही उन सीमाओं को बनाए रखती है जिन्हें हम एक अर्थ में व्यक्तित्व के लिये आवश्यक कह सकते हैं। दूसरी अवस्था में तुम व्यक्तित्व की सीमाओं में आये बिना उसके (व्यक्तित्व के) गुणों से लाभ उठा सकते हो।
क्लेशो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ।। ५।।
५. जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है उनके लिए कठिनाई (मनोव्यथा) अधिक होती है; क्योंकि देहधारी जीवों द्वारा अव्यक्त की प्राप्ति अवश्य ही दुष्कर और कष्टकर है।
और यह नहीं मान लेना चाहिए कि क्योंकि यह अधिक दुष्कर है, इसलिए यह एक उच्चतर एवं अधिक फलप्रद पद्धति है। गीता का सुगमतर मार्ग उसी चरम मोक्ष की ओर अधिक तेजी से, अधिक स्वाभाविक और सहज रूप से ले जाता है।.... ऐकांतिक ज्ञानमार्ग का योगी अपनी प्रकृति की बहुविध माँगों के साथ एक दुःखदायी संघर्ष को अपने ऊपर लाद लेता है; यहाँ तक कि वह उन माँगों को उनकी उच्चतम तृप्ति प्रदान करने से भी इन्कार करता है और अपनी आत्मा के ऊर्ध्वमुख आवेगों को भी काट फेंकता है जब वे संबंधों को इंगित करते हैं या एक निषेधकारी निरपेक्ष तक पहुँचने में न्यून रह जाते हैं। इसके विपरीत, गीता का जीवंत मार्ग हमारी सत्ता की अत्यंत तीव्र प्रवृत्ति को ढूँढ़ निकालता है और उसे ईश्वर की ओर मोड़ कर ज्ञान, संकल्प, भावना और पूर्णत्व की सहज-प्रवृत्ति को आरोही मोक्ष के इतने सारे सशक्त पंखों के रूप में प्रयोग करता है।.... वह अनिर्देश्य एकत्व उन सब को स्वीकार तो करता है जो उसकी ओर आरोहण करते हैं, परंतु आरोही को न तो किसी प्रकार की संबंधात्मक सहायता प्रदान करता है और न उसे पैर टिकाने की जगह ही देता है। सब कुछ कठोर तपस्या और कठिन तथा अकेले वैयक्तिक पुरुषार्थ के द्वारा ही करना होता है। पर जो गीता के बताए तरीके से पुरुषोत्तम की खोज करते हैं, उनके लिए यह सब कितना भिन्न है! जब वे एक ऐसे योग के द्वारा उनका ध्यान करते हैं जो वासुदेव के सिवा और किसी को नहीं देखता, क्योंकि वह सबको उन्हीं के रूप में देखता है, तब वे उन्हें प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक क्षण में, सदा-सर्वदा अपने अगणित रूपों तथा आकृतियों के साथ मिलते हैं, उनके भीतर ज्ञान के दीपक को ऊपर उठाते हैं तथा उसकी दिव्य और सुखद ज्योति से संपूर्ण सत्ता को परिप्लावित कर देते हैं। उसने दिव्या कित होकर वे प्रत्येक रूप तथा आकार में परमात्मा को देख लेते हैं समस्त प्रकृति के द्वारा प्रकृति के अधीश्वर को प्राप्त करते हैं, सब भूतों के द्वारा करते हैं, 'अपने-आप' के द्वारा, वे भी हैं, उस सबकी आत्मा को प्राप्त करते हैं; अबाध रूप से वे एकाएक ही सैंकड़ों उद्घाटित होते तरीकों से उसमें प्रवेश पाते हैं जिससे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इसके विपरीत कठिन संबंधशून्य निस्तब्धता की पद्धति समस्त कर्म से परे हटने का यत्न करती है यद्यपि देहधारी प्राणियों के लिए ऐसा करना असंभव है।
सामान्य तौर पर योगियों, तपस्वियों आदि को हम देखते हैं कि किस प्रकार वे कठोर अनुशासनों का पालन करते हैं, जैसे कि केवल कंद-मूल आदि पर निर्वाह करना, एकदम अल्पाहारी होना, किन्हीं भी शारीरिक सुविधाओं की कुछ भी परवाह न कर के बलपूर्वक अपने आप को विषम परिस्थितियों में रखना आदि। परंतु यह सब कर के भी आवश्यक नहीं कि उन्हें किसी भी सच्ची चीज की प्राप्ति हो।
प्रश्न : इस दुष्कर और कठिन मार्ग का चयन करना भी तो व्यक्ति के अपने वश में नहीं होता। वह भी अपनी प्रकृति के अधीन होकर ही तो ऐसे मार्ग का चयन करता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सरल मार्ग के होते हुए कठिन मार्ग का चयन क्यों करेगा?
उत्तर : यदि हम परमात्मा की क्रिया को ऐसे किसी मानसिक सूत्र में बाँधने का प्रयास करें तो फिर चयन का तो कोई आधार ही नहीं रहेगा। तब तो फिर हम यह भी कह सकते हैं कि कोई आतंकवादी भो उसे भगवान् ने जो प्रकृति प्रदान की है उसी के प्रभाव से आतंकी गतिविधियाँ करता है। और कोई चोर या डाकू भी अपनी प्रकृति के कारण वैसा करता है। परंतु यह एक बेतुका तर्क है और एक ऐसा मानसिक सूत्र है जो हमें बेड़ियों में बाँधकर किसी भी विवेकपूर्ण निर्णय के लिए असमर्थ बना देता है। इसीलिए हमारे ऋषि देश-काल-पात्र पर बल दिया करते थे और उसी के अनुसार किसी भी चीज का निर्णय किया करते थे कि क्या किया जाना चाहिये। क्योंकि श्री अरविन्द कहते हैं कि किसी भी मानसिक सूत्र का विपरीत भी उसके अपने समय और स्थान पर उतना ही सही होता है। बड़े से बड़ा सिद्धांत भी समय पाकर निष्प्रभावी हो जाता है और कोई अन्य सिद्धांत उसका स्थान ले लेता है। अतः अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर जो लोग उस कठोरतर मार्ग का अनुसरण करते हैं इसमें कोई भी दोष की बात नहीं है, परंतु समस्या तो तब आती है जब व्यक्ति सभी के लिए एकमेव उसी मार्ग के अनुसरण पर आग्रह करता है और उस आग्रह से भी एक कदम आगे जाकर बलप्रयोग के द्वारा इसे दूसरों पर थोपने की बात करता है। इसलिए यदि व्यक्ति कहता है कि परमात्मा ने उसे अमुक प्रकृति प्रदान की है और उस कारण वह उसके अनुरूप मार्ग का चयन करता है तो इस बात में कोई दोष नहीं है। परंतु इसके साथ ही साथ उसमें यह नमनीयता और बोध भी होना चाहिये कि परमात्मा ने दूसरों को भिन्न-भिन्न प्रकृतियाँ प्रदान की हैं और उन्हें अपने मार्ग का तब तक पूरी स्वतंत्रता के साथ अनुसरण करने की छूट है जब तक कि वे अन्य किसी की स्वतंत्रता का हनन न करते हों।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।। ६॥
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ।। ७।।
६-७. किन्तु जो लोग अपने समस्त कमाँ को मेरे अर्पण करके और पूर्ण रूप से मेरे परायण होकर अडिग या अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जो अपनी संपूर्ण चेतना को मेरे ऊपर केंद्रित करते हैं, हे पार्थ! उन्हें मैं अविलम्ब ही मृत्युरूप संसार सागर से मुक्त कर देता हूँ।
यहाँ सभी कर्म कर्म के परम प्रभु के प्रति उत्सर्ग कर दिये जाते हैं और वे प्रभु परम संकल्प-शक्ति के रूप में हमारे यज्ञ के संकल्प से मिलते हैं, उससे उसका भार ले लेते हैं और हमारे अंदर स्थित दिव्य प्रकृति के कार्यों का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य के तथा समस्त प्राणियों के प्रेमी और सखा का भक्त प्रेम के उच्च आवेग में अपनी चेतना के संपूर्ण अंतस्तल को और आनंद की समस्त उत्कंठा को उन परमात्मा की ओर लगा देता है तब वे शीघ्र ही रक्षक और उद्धारक के रूप में उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं और उसके मन, हृदय और देह का सुखद आलिंगन करके उसे इस मर्त्य प्रकृति के अंदर मृत्यु-सागर की लहरों से उबारकर सनातन के सुरक्षित वक्षस्थल में ऊपर उठा ले जाते हैं। इसलिए यही सबसे अधिक दुत, विशाल और महान् मार्ग है।
प्रश्न : यहाँ मृत्यु-सागर की लहरों से उबारने का जो उल्लेख हुआ है उसका संकेत क्या मोक्ष प्राप्ति की ओर है?
उत्तर : संसार-सागर अथवा भव-सागर से ऊपर उठने का तो हमारे अनेकों सद्ग्रंथों में उल्लेख आता ही है परंतु इसका तात्पर्य केवल मोक्ष प्राप्ति से ही नहीं है। आध्यात्मिकता का तो अर्थ ही यही है कि हम इस सतही पार्थिव चेतना से उठकर हमारे सच्चे स्वरूप में जाएँ। हमारे ऋषियों का मूल मंत्र ही 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय' रहा है। इसमें मृत्यु से ऊपर उठने का तात्पर्य दैहिक अमरता से नहीं है। अमरत्व का सच्चा अर्थ उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही आत्मा की यात्रा में घटनाएँ मात्र रह जाती हैं और वह इनसे प्रभावित हुए बिना दोनों को ही उपयोग में ले सकता है। संसार-सागर से हमें भय इसलिए होता है क्योंकि हमारी चेतना इससे आसक्त और बद्ध है। जब चेतना इससे मुक्त हो जाती है तब वह व्यक्ति इस भय से मुक्त हो जाता है। सच्चे रूप में कहें तो हमें यह फँसाव इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने अहं से तदात्म हैं और अपने आप को केवल अपनी बाहरी प्रकृति मान बैठते हैं जबकि वास्तव में तो हमारी आत्मा, जो कि हमारे अंदर विराजमान स्वयं दिव्य सत्ता है वह एक सचेतन चुनाव करके इस पार्थिव अभिव्यक्ति में आई है इसलिए इसमें फँसने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि इसे फँसना ही कहें तब तो फिर परम प्रभु स्वयं ही तो इसमें फंसे हुए हैं। संभवतः हम तो अवश रूप से इस अभिव्यक्ति से बद्ध हो सकते हैं परंतु परम् प्रभु की ऐसी कोई बाध्यता प्रतीत नहीं होती कि वे अपनी ही अभिव्यक्ति में बंधेंगे। हमारी संस्कृति में सदा ही यह भान रहा है कि परम् प्रभु केवल अपने आनंद के लिए ही यह सारी जगत् अभिव्यक्ति करते हैं और स्वयं ही इसमें भाग लेते हैं। अब यदि अहं के दृष्टिकोण को छोड़कर हम भी अपने सच्चे भाग से तदात्म हो सकें, अपने अंदर विराजमान भगवान् से एक हो सकें तो हम भी इस आनंद में सहभागी हो सकते हैं और यही इस अभिव्यक्ति का सच्चा उद्देश्य है। योग का यही उद्देश्य है कि वह हमें हमारी वर्तमान स्थिति से उठाकर हमारी सच्ची स्थिति में ले जाता है। यही यज्ञ का आरोहण है। आरंभ में हमारी क्रमविकासमय प्रकृति के प्रभाव से हम इच्छा, कामना, भय आदि के वशीभूत हो कर्म करते हैं। परंतु धीरे-धीरे जब हम अपनी इच्छा की बजाय भगवान् की इच्छा के निमित्त कर्म करने लगते हैं तो हमारा यज्ञ आरंभ हो जाता है। और धीरे- धीरे यह यज्ञ हमारे अधिकाधिक भागों को अपने में समाहित कर लेता है और उन्हें शुद्ध बनाकर इच्छा और कामना आदि की अभिव्यक्ति की बजाय भागवत् कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन बना देता है और तब यज्ञ का सारा भार परमात्मा स्वयं ही ले लेते हैं और व्यक्ति को किसी निजी प्रयास का भान नहीं होता।
प्रश्न : क्या इसे ही जन्म-मृत्यु से छुटकारा कहते हैं?
उत्तर : जन्म-मृत्यु से छुटकारे की बात वह करता है जो इसमें फँसा होता है। ऊपर उठने से तात्पर्य जन्म-मृत्यु के भय से छुटकारा है न कि जन्म-मृत्यु से। जब परमात्मा स्वयं कहते हैं कि 'आत्मानं सृजाम्यहम्' तब इसका क्या यह अर्थ हुआ कि स्वयं वे ही जन्म-मृत्यु से बँधे हुए हैं। इसी प्रकार अनेक सिद्ध पुरुषों ने कहा है कि उन्हें अपने व्यक्तिगत मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं है। वे तो तब तक जन्म लेते रहने को तैयार हैं जब तक कि एक भी आत्मा को पृथ्वी पर सहायता की आवश्यकता होगी। इस सब से यह पता लगता है कि यह वास्तव में जन्म-मृत्यु की बाध्यता और उसके भय से छुटकारा है न कि स्वयं जन्म और मृत्यु से।
यदि हमारे भीतर किसी भी प्रकार की स्पृहा है, चाहे वह मोक्ष की ही क्यों न हो, तो यह इसका सूचक है कि हम एक सच्ची स्थिति में नहीं हैं। क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज की चाह करते हैं वैसे ही यह हमारे अभाव को दर्शाता है जबकि आत्मा की सच्ची स्थिति में उसे किसी चीज की चाह नहीं हो सकती, किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता क्योंकि वह तो स्वात्मलीन होती है और स्वतः आनंदमय होती है जिसका आनंद किन्हीं भी बाहरी चीजों पर आधारित नहीं होता। इसीलिए भगवान् किसी इच्छा के वशीभूत होकर नहीं अपितु अपने संकल्प के द्वारा कार्य करते हैं जबकि इच्छा तथा कामना करना अहंमय चेतना का स्वभाव है। तभी तो भगवान् कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी उन्हें प्राप्त करने की कोई चाह हो परंतु फिर भी लोकसंग्रह के लिए, अपने संकल्प की अभिव्यक्ति के लिए ही वे कर्म में रत रहते हैं। इसीलिए हमारे सभी सद्ग्रंथ भगवान् की सभी क्रियाओं को भगवान् की कृपा की ही अभिव्यक्ति मानते हैं। जब भगवान् श्रीकृष्ण किसी राक्षस का वध भी करते हैं तो हमारे पुराण उसे भगवान् की परम कृपा की अभिव्यक्ति ही मानते हैं और कहते हैं कि भगवान् जिनका वध करते हैं उनका परम उद्धार कर देते हैं और उन्हें वह गति प्रदान करते हैं जो कदाचित् योगियो और तपस्वियों को भी दुर्लभ है। यह पहलू हमारी मानवीय मन-बुद्धि के लिए समझ पाना संभव नहीं है क्योंकि उस चेतना का हमें कोई आस्वादन ही प्राप्त नहीं हुआ है जहाँ बिना किसी अहं के शुद्ध रूप से केवल अपने संकल्प की अभिव्यक्ति के लिए, अपने स्वयं के आनंद की अभिव्यक्ति के लिए ही कर्म किया जाता हो। अतः हमारे लिए करने योग्य श्रेष्ठ कार्य तो यह है कि भगवान् पर विश्वास कर के, उनमें श्रद्धा रख कर अपना सभी कुछ उन्हें समर्पित कर दें।
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ।। ८।।
८. मेरे ऊपर अपने संपूर्ण मन को स्थापित कर और मेरे अंदर अपनी समस्त बुद्धि को स्थित कर; इसमें संशय मत कर कि इस (मर्त्य अस्तित्व) से ऊपर उठकर तू मुझ में ही निवास करेगा।
परमेश्वर मानव-आत्मा से कहते हैं, अपने संपूर्ण मन और बुद्धि को मुझमें स्थित कर देः मैं उन्हें दिव्य प्रेम, संकल्प और ज्ञान की स्वर्गीय ज्योति से परिप्लुत करके अपनी ही ओर, जहाँ से ये सब चीजें प्रवाहित होती हैं, ऊपर उठा ले जाऊँगा। इस मर्त्य जीवन से ऊपर तू मेरे अंदर ही निवास करेगा, इस विषय में संशय मत कर। सीमा में बाँधने वाली पार्थिव प्रकृति की जंजीर शाश्वत प्रेम, संकल्प और ज्ञान के आवेग, उसकी शक्ति और ज्योति के द्वारा ऊपर उठी हुई अमर आत्मा को जकड़ कर नहीं रख सकती।
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय ।॥ ९॥
९. हे धनञ्जय! यदि किसी तरह तू मुझ में अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक स्थिर करने में समर्थ नहीं है तो अभ्यासयोग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा (प्रयत्न) कर।
इसमें संदेह नहीं कि इस मार्ग में भी कठिनाइयाँ हैं; क्योंकि यहाँ भी अपने प्रचंड या स्थूल अधोमुख आकर्षण से युक्त निम्नतर प्रकृति रहती है जो आरोहण की गति का प्रतिरोध करती है और उससे संघर्ष करती है और उन्नयन तथा ऊर्ध्वमुख हर्षोल्लास के पंखों को अवरुद्ध कर देती है। आरंभ में महान् विलक्षण क्षणों में या शांत और उत्कृष्ट समयों में भी यदि दिव्य चेतना प्राप्त होती है, तो भी उसे न तो एकाएक पूर्ण रूप से धारण किया जा सकता है और न ही इच्छानुसार उसको पुनः बुलाया ही जा सकता है; व्यक्तिगत चेतना को दृढ़तापूर्वक भगवान् पर एकाग्र रख सकना प्रायः ही असाध्य प्रतीत होता है; प्रकाश से निर्वासन की लंबी निशाएँ आती हैं, विद्रोह, संदेह या विफलता की घड़ियाँ अथवा क्षण आते हैं। परंतु फिर भी योगाभ्यास के द्वारा तथा अनुभव की सतत् पुनरावृत्ति के द्वारा वह उच्चतम आत्मा हमारी सत्ता पर हावी होती जाती है और हमारी प्रकृति को स्थायी रूप से अपने अधिकार में ले लेती है।
अभ्यासे ऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ।। १० ।।
१०. यदि तू योग के अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिये कर्म परायण (कर्म करनेवाला) हो; सभी कर्म मेरे हित करते हुए तू अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त कर लेगा।
क्या ऐसा करना भी मन की बहिर्मुख प्रवृत्ति के बल और आग्रह के कारण अत्यंत कठिन पाया जाता है? तो इसका एक सरल उपाय है, सभी कर्मों को कर्म के स्वामी के हित करना, ताकि मन की प्रत्येक बहिर्मुख प्रवृत्ति हमारी सत्ता के आंतर आध्यात्मिक सत्य से संबद्ध हो जाए और उसे अपनी क्रियाशीलता के समय भी नित्य सद्वस्तु की ओर पुनः बुलाया जा सके और अपने उद्गम के साथ संबद्ध किया जा सके। तब, पुरुषोत्तम की उपस्थिति प्रकृतिगत मनुष्य के अंदर तब तक बढ़ती जायेगी जब तक कि वह उससे परिपूरित होकर एक देवता और आत्मा ही नहीं बन जाता; संपूर्ण जीवन ईश्वर का सतत् स्मरण बन जाएगा और पूर्णता भी वर्धित होगी और उसके साथ ही वर्धित होगा मानव आत्मा की संपूर्ण सत्ता का परम सत्ता के साथ एकत्व भी।
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ।। ११ ।।
११. किन्तु यदि यह करने में भी तू असमर्थ है तो मेरे योग का आश्रय लेकर, अपनी (निम्न) आत्मा को संयत करके समस्त कर्मों के फल का त्याग कर।
परन्तु हो सकता है कि ईश्वर का यह सतत् स्मरण तथा अपने कार्यों को उनकी ओर ऊपर उठा ले जाना भी सीमित मन की सामर्थ्य से परे की वस्तु प्रतीत हो, क्योंकि मन अपनी भूलने की प्रवृत्ति में कार्य तथा उसके बाह्य उद्देश्य की ओर मुड़ जाता है और तब उसे भीतर देखना तथा हमारी प्रत्येक चेष्टा को आत्मा की दिव्य वेदी पर उत्सर्ग करना याद नहीं रहता। ऐसी दशा में उपाय यह है कि कर्म में निम्नतर 'स्व' को संयमित करके फल की कामना के बिना कर्म किये जाएँ। समस्त फल का त्याग करना होगा, उसे कर्म का संचालन करनेवाली शक्ति को सौंप देना होगा और फिर भी, उस शक्ति द्वारा हमारी प्रकृति पर आरोपित किये गये कार्य को करना ही होगा। क्योंकि, इस साधन के द्वारा बाधा निरंतर घटती जाती है और आसानी से दूर हो जाती है, मन को ईश्वर का स्मरण करने तथा भगवच्चेतना के स्वातंत्र्य पर अपने-आप को एकाग्र करने का अवकाश प्राप्त हो जाता है। यहाँ गीता क्षमताओं की एक चढ़ती हुई श्रृंखला का प्रतिपादन करती है और कर्मों के इस योग को सर्वोच्च महत्त्व प्रदान करती है।
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते ।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ।। १२ ।।
१२. अवश्य ही अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है; ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठतर है; ध्यान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है; कर्मफल त्याग के तुरंत बाद शांति प्राप्त हो जाती है।
अभ्यास, अर्थात् किसी पद्धति का अनुशीलन करना, किसी प्रयत्न को और अनुभव को बारंबार दोहराते रहना एक महान् और शक्तिशाली साधन है, परंतु इससे श्रेष्ठतर है ज्ञान, अर्थात् विचार का सफलतापूर्वक और प्रकाशित रूप से वस्तुओं के पीछे के निहित सत्य की ओर मुड़ना। इस विचारात्मक ज्ञान से भी बढ़कर है सत्य के ऊपर शांत और पूर्ण एकाग्रचित्तता जिससे कि अंततः चेतना उसमें निवास करने लगे और उससे सदा एकीभूत रहे। परंतु उससे भी अधिक प्रभावशाली है अपने कर्मों के फल का त्याग क्योंकि वह तुरंत ही विक्षोभ या अशांति के सभी कारणों को नष्ट कर डालता है और स्वतः ही एक आंतरिक शांति एवं स्थिरता को लाता तथा सुरक्षित बनाए रखता है, और शांति एवं स्थिरता ही वह आधार है जिस पर अन्य सब कुछ पूर्णत्व लाभ करता है और शांत आत्मा के द्वारा अधिकृत होकर सुरक्षित हो जाता है। तब चेतना निश्चिंत हो सकती है, अपने-आप को प्रसन्नतापूर्वक भगवान् में स्थिर करके निर्विघ्न रूप से पूर्णता की ओर उठ सकती है। और, तभी ज्ञान, संकल्प और भक्ति अपने शिखरों को ठोस शांति की दृढ़ भूमि से नित्यता के आकाश में उठा ले जा सकते हैं।
तब फिर, जिस भक्त ने इस मार्ग का अनुसरण किया है और शाश्वत की उपासना की ओर मुड़ा है, उसकी दिव्य प्रकृति क्या होगी, उसकी चेतना और सत्ता की महत्तर स्थिति क्या होगी? गीता कई श्लोकों tilde 4 बदल-बदल कर अनेक प्रकार से अपनी पहली आग्रहपूर्ण माँग को, समता, निष्कामता और आत्मा के स्वातंत्र्य की माँग को गुंजारित करती है। आधार तो सदा यही रहना होगा, - और इसीलिए इस पर आरंभ में इतना अधिक बल दिया गया था। और उस समता में भक्ति, अर्थात् पुरुषोत्तम से प्रेम और उनकी आराधना के द्वारा आत्मा को किसी ऐसी महत्तम एवं उच्चतम पूर्णता की ओर उठाना होगा जिसकी यह स्थिर समता विशाल आधार होगी। इस आधारभूत सम चेतना के कई सूत्र यहाँ बताये गये हैं।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ।। १३ ।।
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ।। १४।।
१३-१४. जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता और करुणा का भाव रखता है, 'मैं' और 'मेरा' के अहंकार से रहित होता है, सुख और दुःख में समचित्त रहने वाला क्षमाशील है, जो योगी सदा संतुष्ट रहता है, आत्म-संयमी और दृढ़ निश्चयी रहता है, और जिसके मन और बुद्धि मुझे समर्पित होते हैं, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है।
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ।। १५।।
१५. जिससे जगत् क्लेशित नहीं होता और जो जीवों से क्लेश का अनुभव नहीं करता और जो हर्ष, आक्रोश और भय के उद्वेगों से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है।
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ।। १६।।
१६. जो कोई अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र, कार्यदक्ष, उदासीन, अव्यथित रहता है, जिसने समस्त कमाँ के आरंभ (प्रवृत्ति) को त्याग दिया है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ।। १७।।
१७. जो न हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है, जिसने शुभ और अशुभ घटनाओं के भेद को दूर कर दिया है, वह भक्ति से परिपूर्ण मनुष्य मुझे प्रिय है।
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।। १८।।
तुल्यनिन्दास्तुतिौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।। १९।।
१८-१९. जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, शीत और उष्ण, सुख और दुःख में समान रहता है, जो आसक्ति से रहित, प्रशंसा और निंदा में सम रहता है, जो मौनी (मितभाषी) है, जो भी कुछ आए उस सबसे संतुष्ट रहता है, किसी घर या रहने के स्थान से आसक्त नहीं रहता, जो स्थिरबुद्धि है, भक्तियुक्त है, वह मुझे प्रिय है।
समता, निष्कामता, निम्नतर अहंकारमय प्रकृति और उसके दावों से मुक्ति सदा ही वे एकमात्र पूर्ण आधार हैं जिनकी गीता महान् मोक्ष के लिए माँग करती है। अंत तक भी गीता बारंबार अपनी प्रथम मूलभूत शिक्षा तथा मूल अभीष्ट विषय पर, सभी वस्तुओं में एक ही आत्मा को देखनेवाली शांत ज्ञानमय आत्मा पर, ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्राप्त होनेवाली शांत निरहंकार समता पर, उस समत्व की अवस्था में कर्मों के प्रभु के प्रति अर्पित निष्काम कर्म पर, मनुष्य की संपूर्ण मानसिक प्रकृति को महत्तर अंतर्वासी आत्मा के हाथों में समर्पण करने पर जोरदार बल देती रहती है। और, इस समता का शिखर या इसकी पराकाष्ठा है ज्ञान पर सुप्रतिष्ठित वह प्रेम जो निमित्तरूप से किये जानेवाले कर्म में चरितार्थ होता है तथा सब वस्तुओं और प्राणियों तक विस्तारित होता है, अर्थात् जो विश्व के स्रष्टा और महेश्वर दिव्य आत्मा, 'सुहृदं 4.29 सर्वभूतानां सर्वलोकमहेश्वरम्' के लिए व्यापक, अनन्य तथा सर्वधारक प्रेम होता है।
यह वह आधार, अवस्था एवं साधन है जिसके द्वारा हमें परमोच्च आध्यात्मिक पूर्णता अर्जित करनी है, और भगवान् कहते हैं कि जो लोग किसी भी प्रकार इससे युक्त हैं वे सभी मेरे प्रिय हैं, भक्तिमान् मे प्रियः। परंतु परमेश्वर की अत्यंत निकटवर्ती वे आत्माएँ मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतीव मे प्रियाः, जिनका मेरे लिए प्रेम उस और भी विशालतर तथा महत्तम पूर्णता के द्वारा पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है जिसका पथ एवं प्रणाली मैंने तुझे अभी बतायी है।
xii. 17, xvii.47
ये तु धर्ष्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ।। २० ।।
२०. परन्तु जो भक्त केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य निर्धारित करके पूर्ण श्रद्धा के साथ, जैसा अभी यहाँ वर्णन किया गया है इस अमरताप्रद धर्म का यथावत् रीति से अनुष्ठान करते हैं वे भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं।
गीता की भाषा में 'धर्म' का अर्थ है सत्ता तथा उसके कर्मों का सहज-स्वाभाविक विधान तथा आंतरिक प्रकृति से निःसृत और उसके द्वारा निर्धारित कर्म, 'स्वभावनियतं कर्म।' मन, प्राण और शरीर की निम्नतर अज्ञ चेतना में अनेक धर्म, अनेक नियम, अनेक मानदंड तथा विधान होते हैं, क्योंकि मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक प्रकृति के अनेक विभिन्न निर्धारण तथा प्रकार हैं। अमर धर्म एक ही है; वह सर्वोच्च आध्यात्मिक दिव्य चेतना तथा उसकी शक्तियों का, परा प्रकृतिः का, धर्म है। वह तीनों गुणों से परे है, और उस तक पहुँचने के लिए इन सब निम्नतर धर्मों का परित्याग करना होगा, 'सर्वधर्मान् परित्यज्य।' उनके स्थान पर शाश्वत की अखंड, मोक्षप्रद एकीकारक चेतना तथा शक्ति को ही हमें अपने कर्म का अनंत उद्गम, उसका साँचा, निर्धारक तथा प्रतिमान बनाना होगा। अपने निम्नतर वैयक्तिक अहंभाव से ऊपर उठना, निर्विकार सनातन सर्वव्यापी अक्षर पुरुष की निर्वैयक्तिक और सम-स्थिरता में प्रवेश करना और फिर उस स्थिरता से, अपनी समस्त सत्ता और प्रकृति के पूर्ण आत्मसमर्पण के द्वारा, उस पूर्ण स्थिरता के लिए अभीप्सा करना जो अक्षर से अलग और उच्चतर है - यह इस योग की पहली आवश्यकता है। इस अभीप्सा के बल पर मनुष्य अमर धर्म की ओर उठ सकता है। वहाँ, महत्तम 'उत्तम पुरुष' के साथ सत्ता, चेतना और दिव्य आनंद में एक होकर, उनकी परमोच्च क्रियाशील प्रकृति-शक्ति, 'स्वां प्रकृतिः', के साथ एक होकर मुक्त आत्मा उच्चतम अमरत्व तथा पूर्ण स्वातंत्र्य की वास्तविक शक्ति के साथ अनंत रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकती है, असीम रूप से प्रेम कर सकती है और अचूक रूप से कर्म कर सकती है। शेष गीता इस अमर धर्म पर अधिक पूर्ण प्रकाश डालने के लिए ही लिखी गयी है।
xvii. 66
अमर धर्म वह है जिसमें व्यक्ति अक्षर ब्रह्म को नहीं अपितु केवल पुरुषोत्तम परमात्मा को अंतिम उद्देश्य मानकर उनकी ओर चलता है। जो लोग भगवान् पुरुषोत्तम को ही अपना संपूर्ण आधार मानते हैं और उनकी ओर गति करते हैं वे ही सच्चे धर्म की राह पर हैं और ऐसे भक्तों को ही वे प्राप्त होते हैं। अतः इस प्राप्ति में भक्ति को ही सर्वोच्च स्थान और महत्ता प्रदान की गई है।
प्रश्न : सोलहवें श्लोक में कहा गया है कि 'जिसने सब कमाँ के आरम्भ को त्याग दिया है', इसका क्या अर्थ है?
उत्तर : कर्मों के आरंभ को त्याग देने का अर्थ है कि इच्छा या कामना के वशीभूत हो कर्म न करना अपितु भगवद्-प्रेरणा के अनुसार कर्म करना। जब हम अपने अहं की बजाय भगवद् संकल्प की अभिव्यक्ति के अनुसार क्रिया करते हैं तब हम सर्वारंभपरित्यागी होते हैं क्योंकि तब कर्म का उत्प्रेरण भगवान् के द्वारा होता है और इस कारण वे कर्म हमें बाँधते नहीं। दिव्य कर्मी के लक्षणों में हम यह चर्चा कर ही चुके हैं कि उसके द्वारा दिव्य प्रकृति जो भी कर्म कराती है, जो भी भाव लाती है, जो भी विचार लाती है उन सभी में वह सदा ही आनन्दित रहता है। कर्म से उसकी कोई लिप्तता अथवा बाध्यता होती ही नहीं क्योंकि वह तो उन सब से ऊपर होता है। इस कारण उन कर्मों का उस पर कोई कार्य-कारण प्रभाव नहीं होता। इसीलिए दिव्य कर्मी को 'सर्वारंभपरित्यागी' अर्थात् सभी आरम्भों के त्यागी की संज्ञा दी जाती है। वह किसी कार्य का आरम्भ नहीं करता। उसकी कोई स्वतंत्र व्यक्तिगत इच्छा रहती ही नहीं। उसके कर्म दिव्य प्रकृति के द्वारा ही चालित होते हैं। जिस समय जैसी आवश्यकता होती है वैसा उसके विचार आ जाता है, वैसा ही उसके द्वारा कर्म हो जाता है। इसलिये जब कर्मों का कर्त्ता वह स्वयं नहीं रहता तब फिर मानसिकता में कर्म-जनित कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होती। उसको सत्ता पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति खुली होती है और उन्हें समर्पित होती है और वह स्वयं को ब्रह्मस्वरूप जान लेता है।
प्रश्न : जैसा कि भगवान् कहते हैं कि जो भक्त इस अमरताप्रद धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे मुझे प्रिय हैं। जब एक बार व्यक्ति एकमात्र परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है तब फिर क्या केवल अमर धर्म ही बचता है, परोपकारिकता आदि अन्य धर्म अप्रासंगिक हो जाते हैं?
उत्तर : इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। जब व्यक्ति भागवत् संकल्प के साथ युक्त होता है तभी सच्चे रूप में सभी धर्मों का निर्वाह होता है। जब व्यक्ति परमात्मा के साथ युक्त होगा तभी वह सच्चा परोपकार कर सकता है। जो कुछ परमात्मा के द्वारा आता है वही सच्चा धर्म है। आखिर सारे धर्म और आदर्श भी तो इसी आधार पर प्रतिष्ठित होते हैं, परमात्मा के अतिरिक्त तो इनका कोई आधार ही नहीं है। इसलिए परमात्मा से युक्त चेतना में कोई विरोधाभास नहीं रहता क्योंकि तब हर दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ ही होता है।
श्रीअरविन्द ने गीता को तीन षट्कों में विभाजित किया है जिसके अनुसार यह दूसरा षट्क समाप्त हो गया है। तीसरे में मूल रूप से कोई नया तत्त्व नहीं है परंतु पहले आए मूल तत्त्वों का ही विशद निरूपण है जिनका कि पहले उल्लेख तो हुआ था पर जिन्हें पूरी तरह hat H स्पष्ट नहीं किया गया था।
इस प्रकार बारहवाँ अध्याय 'भक्तियोग' समाप्त होता है।
तेरहवाँ अध्याय
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ
निम्नतर प्रकृति से निकल कर दिव्य प्रकृति में आत्मा के ऊपर उठने के मार्ग को एक सुस्पष्ट और पूर्ण ज्ञान पर प्रतिष्ठित करने के लिए गीता अपने अंतिम छः अध्यायों में दिव्य गुरु द्वारा अर्जुन को पहले ही दिये जा चुके ज्ञान को एक दूसरे रूप में पुनः निरूपित करती है। तत्त्वतः तो यह वही ज्ञान है, पर अब इसके ब्यौरों तथा संबंधों को सुस्पष्ट करके उन्हें उनका पूर्ण अर्थ प्रदान किया गया है, जिन विचारों एवं सत्यों का केवल चलते-चलते संकेत कर दिया गया था या किसी अन्य प्रयोजन के प्रकाश में सामान्यतः ही प्रतिपादन किया गया था उनका पूरा-पूरा मूल्य अभी प्रकट किया गया है। इस प्रकार पहले छः अध्यायों में सारी प्रधानता अक्षर आत्मा तथा प्रकृति से आच्छादित आत्मा के पारस्परिक भेद के लिए आवश्यक ज्ञान को ही दी गयी थी। वहाँ परम् आत्मा एवं परम-पुरुष-विषयक जो उल्लेख आए थे वे संक्षिप्त थे और बिल्कुल भी प्रकट या व्यक्त नहीं थे।... परन्तु अब परम् पुरुष, अक्षर आत्मा, जीव तथा कर्मशील त्रिगुणात्मिका प्रकृति के यथार्थ संबंधों को अधिक सुनिश्चित रूप में प्रकट करना आवश्यक है। अतएव अर्जुन से एक प्रश्न कराया जाता है जो अभी तक अर्ध-प्रकाशित इन विषयों पर अधिक विशद प्रकाश डालने का अवसर उपस्थित करेगा।
अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ।
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ १ ॥
१. अर्जुन ने कहाः हे केशव! प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, इन सब को मैं जानना चाहता हूँ।
वह पुरुष और प्रकृति के विषय में जानने की माँग करता है; वह सत्ता के क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में प्रश्न करता है। इसी में आत्मा और जगत् के उस समस्त ज्ञान का सार निहित है जिसकी आत्मा को अब भी आवश्यकता है यदि उसे अपने प्राकृत अज्ञान का उन्मूलन करना है तथा अपने कदमों को ज्ञान, जीवन और कर्मों के, एवं इन वस्तुओं में विद्यमान भगवान् के साथ अपने संबंधों के समुचित उपयोग पर सुदृढ़ करके जगत् के सनातन आत्मा के साथ अपनी सत्ता के एकत्व की ओर आरोहण करना है।
गीता के इस अंतिम षटक् में तत्त्वतः वही ज्ञान है जिसका उल्लेख पहले के अध्यायों में हो तो चुका है परंतु जिसके ब्यौरों का विस्तार से वर्णन करना अभी बाकी है। भगवान् ने अर्जुन को पहले यह बताया अवश्य है कि इस निम्न प्रकृति से निकल कर दिव्य प्रकृति में जाना होगा, परंतु अभी तक उसके मार्ग के विषय में संबंधित ब्यौरों को, उस मार्ग पर आने वाली संभावित चीजों को संकेत भर में ही कहा है, विस्तारपूर्वक स्पष्ट नहीं किया है। आरंभ में भी भगवान् अर्जुन को निखैगुण्य और निर्द्वन्द्व होने का उपदेश करते हैं, परंतु उन स्थितियों का समुचित वर्णन और उससे संबंधित ब्यौरों के विषय में पूरी तरह स्पष्टता अभी आनी बाकी है। इसलिए गीता इन्हीं सब बिन्दुओं का पूर्ण रूप से निरूपण कर के अंत में अपना गुह्यतम वचन 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' प्रकाशित करती है जिसमें सारे योगों, धारणाओं, धर्म के ढाँचों को तोड़ कर वह उन सबको अतिक्रम कर जाती है। आखिर कोई भी योग-पद्धति, कोई भी ज्ञान या दर्शन या अन्य कुछ भी, भले ही अपने आप में कितना ही विशाल क्यों न हो, तो भी व्यक्ति और परमात्मा के बीच के संबंध को, उनके संसर्ग को भला कैसे और कितना परिभाषित या निरूपित कर सकता है? और श्रीअरविन्द के अनुसार गीता द्वारा योग की सभी पद्धतियों को उनके उत्कृष्टतम रूप में अपनाना, उन सब को आपस में समन्वित कर भक्ति में परिणत कर देना और फिर इन सभी को तोड़ कर अंत में इनका पूर्णतः अतिक्रम कर जाना ही इसे इतना महत्त्वपूर्ण बना देता है। क्योंकि वास्तव में तो आखिर आत्मा किन्हीं भी पद्धतियों में बाँधी ही कैसे जा सकती है। वह तो पूर्णतः स्वतंत्र है और अपने स्वयं के विधान के अनुसार चलती है। इसलिए गीता अपनी किन्हीं भी शिक्षाओं तक सीमित नहीं रहती अपितु अंत में 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' कह कर सभी कुछ का अतिक्रम कर के सीधे अतिमानस की भव्यताओं तक ले जाती है। हालाँकि गीता इसके विषय में कुछ भी वर्णन नहीं करती क्योंकि इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, इस स्थिति को तो व्यक्ति को जीना ही होता है, अपनी आत्मा में इसका अनुभव करना होता है। इसलिए अपना परम वचन कह कर गीता उसका कोई स्पष्टीकरण दिये बिना वहीं रुक जाती है। क्योंकि उस स्थिति से पहले जिन स्थितियों का उल्लेख हुआ है वे तो पथसंकेत के रूप में हैं जैसे कि ब्रह्म-निर्वाण, समत्व आदि की स्थितियाँ। परंतु जब कोई विरली ही आत्मा इन सभी पड़ावों को भी पार कर जाती है, सभी धर्मों को, अपने सभी आधारों को तोड़ डालती है, उस स्थिति का कोई वर्णन नहीं हो सकता, वह सभी वर्णनों से परे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस स्थिति में केवल दिव्य विधान ही प्रभावी होता है। हमारे ऊँचे से ऊँचे दर्शन आदि भगवान् को देखने के हमारे मानसिक तरीके मात्र हैं जिनमें भगवान् सीमित नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जब हम उन्हें असीम, अव्यक्त, परम पुरुष आदि संज्ञाएँ भी देते हैं तब भी ये केवल हमारी मानसिक परिभाषाएँ मात्र ही होती हैं और इनसे परमात्मा किसी भी प्रकार सीमित नहीं हो सकते। इसीलिए जब वह दिव्य विधान प्रभावी होता है तब उस स्थिति के विषय में मनुष्य जान ही कैसे सकता है और हमारी मानसिक शब्दावली में उसका निरूपण भी असंभव है। परंतु अपने अहं में हम अपनी क्षुद्रता का बोध खो बैठते हैं और हमें लगता है कि हमसे श्रेष्ठतर तो कोई है ही नहीं। जबकि अतिमानसिक चेतना भी लोकों के स्तरक्रम में वह निम्नतम स्तर है जहाँ आत्मा को अपनी अभिव्यक्ति का पहली बार निर्बाध स्थान मिलता है। आत्मा की भव्यता की सच्ची अभिव्यक्ति तो अतिमानसिक स्तर से भी उच्चतर स्तरों में होती है। वर्तमान में तो स्वयं अतिमानस ही हमारी सामान्य कल्पना के लिए किसी चमत्कार से बढ़कर नहीं है। इसलिए इन स्थितियों का तो वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। श्रीअरविन्द ही वे पहले अग्रणी हैं जिन्होंने अतिमानसिक भूमिका तक की यात्रा तय की है इसलिए उनसे पूर्व तो इसके वर्णन की आशा भी कैसे की जा सकती थी। इसीलिए वे कहते हैं कि चूंकि पहले कोई भी उस मार्ग पर नहीं गया था इसलिए उन्हें बिना किसी पथसंकेत के स्वयं ही उस मार्ग को तैयार करना था। और जब वे अपनी कृतियों में उस मार्ग का कुछ-कुछ वर्णन करते भी हैं, क्योंकि अपने आप में वह इतना वर्णनातीत है कि केवल श्रीअरविन्द के समान कोई दिव्य व्यक्तित्व ही उसके केवल किसी अंशमात्र का वर्णन कर सकता है, और वह भी हमारी किन्हीं भी मानसिक संरचनाओं से इतना परे है कि उसे वास्तव में समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। और अपने सभी वर्णनों में श्रीअरविन्द सदा ही यह भाव रखते हैं कि जो कुछ उन्होंने वर्णन किया है वह भी देखने का एक तरीका मात्र ही है, हालाँकि एक ऐसा तरीका है जो सत्य को अधिक समग्र और अंतरंग रूप से देखता है, तो भी है एक तरीका मात्र ही। इससे हमें यह भान होता है कि अपने आप में परमात्मा का वह सत्य कितने वर्णनातीत रूप से विशाल है।
श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।। २।।
२. श्रीभगवान् ने कहाः हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं; और जो इसे जानता है उसे ज्ञानीजनों के द्वारा क्षेत्रज्ञ कहा जाता है।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।। ३।।
३. हे भारत! सभी क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जान; मेरे मत से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है।
आगे आनेवाली परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल यह स्थूल शरीर ही क्षेत्र नहीं है, अपितु वह सब भी क्षेत्र है जिसे हमारा शरीर आश्रय देता है, अर्थात् प्रकृति का कार्य-व्यापार, मानसिकता, हमारी सत्ता' की वस्तुनिष्ठता (objectivity) और आत्मनिष्ठता (subjectivity) की स्वाभाविक क्रिया। यह विशालतर शरीर भी केवल व्यष्टिगत क्षेत्र ही है; परंतु इस ज्ञाता 'पुरुष' का एक अधिक व्यापक, सार्वभौम, विश्व-शरीर, विश्व-क्षेत्र भी है। क्योंकि, प्रत्येक देहधारी प्राणी में यही एक ज्ञाता विद्यमान हैः प्रत्येक भूत में वह अपनी प्रकृति की शक्ति के इस पृथक् बाह्य परिणाम को, जिसे इसने अपने निवास के लिये विरचित किया है, 'ईशावास्यं इदं सर्वं यत्किञ्च *, मुख्यतया और केंद्ररूप से प्रयोग में लाता है; यह अपनी गतिशील ऊर्जा की प्रत्येक पृथक्, व्यष्टिभूत अपरिवर्तित ग्रंथि या केंद्र को अपने विकासोन्मुख सामंजस्यों का प्रथम आधार और क्षेत्र बनाता है।
_____________________
* उपनिषद् प्रकृति के पाँच प्रकार के शरीर या कोषों का उल्लेख करते हैं, अन्नमय (भौतिक), प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा दिव्य शरीरः इन्हें सम्पूर्ण क्षेत्र, 'क्षेत्रम्', समझा जा सकता है।
* CWSA 17:5
प्रकृति के अन्दर यह जगत् को उस रूप में जानता है जिस रूप में यह इस एक सीमित शरीर में चेतना को प्रभावित करता तथा इसके अन्दर प्रतिबिम्बित होता है; जगत् हमारे लिए उसी रूप में विद्यमान है जैसा वह हमारे पृथक् मन के अंदर दिखायी देता है, – और अन्त में यह छोटी-सी दिखनेवाली देहबद्ध चेतना भी अपने को इतना विस्तृत कर सकती है कि यह अपने अन्दर संपूर्ण विश्व को समा ले, आत्मनि विश्वदर्शनम्। परन्तु, भौतिक रूप में, यह ब्रह्माण्ड में एक पिण्ड मात्र ही है, और ब्रह्माण्ड भी, यह विशाल विश्व भी, एक देह एवं क्षेत्र है जिसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा निवास करता है।
यह बात तब स्पष्ट हो जाती है जब गीता हमारी सत्ता की इस गोचर देह के स्वरूप, प्रकृति एवं उद्गम, विकारों एवं शक्तियों का निरूपण करने की ओर अग्रसर होती है।
यहाँ हमें यह स्पष्ट होना चाहिये कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। बिना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। जब कोई जानने वाला ही नहीं है तब फिर संभूति का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार यदि संभूति ही नहीं है तो फिर जानने वाले का भी कोई अर्थ नहीं है। क्षेत्र वह है जो जाना जाता है और क्षेत्रज्ञ वह है जो जानता है। यह अकाट्य नियम है कि इन दोनों के बिना अभिव्यक्ति संभव ही नहीं है। यह एक मूलभूत सत्य है। इसी को हम पुरुष और प्रकृति कह देते हैं।
जो कुछ भी हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, और जो कुछ हम कभी भविष्य में जानेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे वह सभी क्षेत्र है। इसलिए मानसिक, अतिमानसिक, विज्ञानमय, आनन्दमय सभी जगत् क्षेत्र ही हैं। और इन सब को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इसलिये वस्तुतः केवल परमात्मा ही एकमात्र क्षेत्रज्ञ हैं। वे ही समस्त क्षेत्र के एकमात्र ज्ञाता हैं, परंतु वे किन्हीं भी साधनों से ज्ञेय नहीं हैं। और उनके जिस भी अंश को जान लिया जाता है वह क्षेत्र बन जाता है क्योंकि केवल क्षेत्र को ही जाना जा सकता है न कि स्वयं परमात्मा को। प्रभु के बारे में जो कुछ भी ऊँचे से ऊँचा हम जान सकते हैं वह सब क्षेत्र का ही अंग है। परमात्मा कहते हैं कि सभी चीजों में क्षेत्रज्ञ केवल वे स्वयं ही हैं। हालाँकि क्षेत्रज्ञ अपने आप को व्यष्टि पुरुष के भाव में स्थित कर के उस दृष्टिकोण से जान सकते हैं, अपने आप को अन्य किसी भाव में स्थित करके उस अन्य दृष्टिकोण से भी जान सकते हैं। परंतु भले वे कोई भी भाव क्यों न अपनाएँ, वह होता उस एकमेव क्षेत्रज्ञ का ही रूप है। और यह भाव जितना ही गहरा और ऊँचा होगा उतने ही अधिक क्षेत्र का वह ज्ञाता होगा।
इस अभिव्यक्ति में ऐसा कुछ नहीं है जो पुरुष और प्रकृति के सायुज्य के बिना बना हो। और इस सबके पीछे स्वयं माँ जगदम्बा विराजमान हैं। अतः सब कुछ क्षेत्र ही है, जबकि वह ज्ञाता इतना सूक्ष्मातिसूक्ष्म है कि सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी पकड़ में नहीं आता। असंख्यों ब्रह्माण्ड और अनेकानेक स्तरीय सृष्टि का निर्माण केवल उन्हीं ज्ञाता को अभिव्यक्त करने का ही तो प्रयास है परंतु ज्यों ही उसकी अभिव्यक्ति होती है त्यों ही वह क्षेत्र बन जाता है और क्षेत्रज्ञ उसमें से बच निकलता है। इसी कारण हम ऐसी अद्भुत सृष्टि देखते हैं। हमारे मानवीय दृष्टिकोण से हमें इस रूप में यह सारा जगत् व्यापार दिखाई देता है। वास्तव में इसका क्या स्वरूप होगा यह तो कोई भी नहीं कह सकता। परंतु चूँकि हमारे ऋषियों ने इसका इस रूप में वर्णन किया है अतः हमारे लिए तो वही परम सत्य है और फिर श्रीअरविन्द द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद तो इसमें संदेह का कोई कारण भी नहीं रह जाता।
भगवान् की पराप्रकृति भी सदा ही उन्हें अभिव्यक्त करने का पूरा प्रयास करती रहती है परंतु वे तो उसके हर प्रयास में से बच निकलते हैं। समस्त देवता, राक्षस, सभी स्थूल या सूक्ष्म लोक और उनकी सभी सृष्टियाँ आदि सभी क्षेत्र में ही आते हैं। और यह सब होते हुए भी वे स्वयं ही क्षेत्र भी हैं क्योंकि उनके अतिरिक्त तो अन्य किसी चीज की कोई स्वतंत्र विद्यमानता हो ही नहीं सकती। यह तो मात्र हमारा मानवीय दृष्टिकोण है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच भेद करता है क्योंकि भगवान् के अलावा तो अन्य किसी को कोई सत्ता ही नहीं है, अतः वस्तुतः वे स्वयं ही स्वयं का अवलोकन करते हैं।
श्रीअरविन्द अपने सावित्री महाकाव्य में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार यह सारी सृष्टि और कुछ नहीं केवल परमात्मा और उनकी पराशक्ति के बीच एक खेल है। भगवान् की पराशक्ति या फिर परा-प्रकृति परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए एक से एक अद्भुत लोकों का, एक से एक अद्भुत रूपों का सृजन करती है और परमात्मा उन सब से बच निकलते हैं। परंतु परमात्मा और उनकी परा-प्रकृति का आपस में इतना अंतरंग रूप से प्रेम है कि परा-प्रकृति की प्रसन्नता के लिए वे एक क्षुद्र से क्षुद्र वस्तु भी बनने को तैयार रहते हैं और परा-प्रकृति सदा उन्हीं को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती रहती हैं। इसलिए सभी कुछ पूर्ण रूप से स्वयं परमात्मा का ही रूप है परंतु फिर भी परमात्मा स्वयं किसी भी रूप से अनंततः परे भी हैं। इस अंतरंग प्रेम के कारण ही हमारे अंदर का आत्म-तत्त्व सदा ही जगदंबा से घनिष्ठ रूप से प्रेम करता है और इस प्रेम को संसिर करना, इसे चरितार्थ करना ही जीवन का सच्चा सार है। और इस संपूर्ण सृष्टि का मूलभूत सत्य यही है कि परमात्मा और उनकी चित्-शकि जगदंबा के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है और आपस में ये अंतरंगतम प्रेम में हैं। यह कोई तात्विक या दार्शनिक सत्य नहीं अपितु सभी कुछ का मूल सत्य है, सब कुछ का आधार है। इस संबंध का सर्वत्र अनुभव कोई विरली ही आत्मा कर सकती है क्योंकि यह संबंध तो सभी कुछ की पराकाष्ठा है। वास्तव में तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई आकर्षण होता है वह उन्हीं के बीच के आकर्षण की एक छाया है। और जिस हद तक परमात्मा और परा-प्रकृति के बीच की क्रिया हमारे अंदर संसिद्ध हो पाती है उसी हद तक हम उसकी प्रगाढ़ता को अनुभव कर पाते हैं, उस हद तक हमारा जीवन ऊपर उठ जाता है। यह भी एक देखने का तरीका मात्र ही है। इस प्रकार हम सारे ब्रह्माण्ड को यज्ञ के आरोहण, ज्ञान के आरोहण, प्रेम के आरोहण, आनन्द के आरोहण, परम आकर्षण के आरोहण के रूप में देख सकते हैं। हमारा वैष्णव तंत्र सभी कुछ का वर्णन राधा और कृष्ण के बीच, विष्णु और लक्ष्मी के बीच की क्रीड़ा के रूप में ही करता है। स्वयं श्रीअरविन्द व श्रीमाताजी ने कहा है कि उनके अंदर दो शरीरों में एक ही आत्म-तत्त्व की, एक ही चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्त्व सभी कुछ का सार है।
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत् ।
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ।। ४।।
४. वह क्षेत्र क्या है और उसका स्वभाव, उसका उद्गम और उसके विकार क्या हैं, और वह (क्षेत्रज्ञ) क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उस सबको संक्षेप में मुझ से सुन।
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ।
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ।। ५।।
५. इसे ऋषियों के द्वारा अनेक तरीकों से और विविध प्रकार के छन्दों में अलग-अलग रूपों में तथा युक्तियुक्त और निर्णायक ब्रह्मसूत्रों के पदों के द्वारा भी गाया गया है।
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ।। ६।।
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ।। ७।।
६-७. अव्यक्त (मूल प्रकृति), पंच महाभूत, दस इंद्रियाँ और एक मन, बुद्धि और अहंकार, तथा पाँच इंद्रियों के विषय (तन्मात्रा), राग और द्वेष, सुख और दुःख, संघात, चेतना और धृति (दृढ़ता), इन सब को मिलाकर क्षेत्र तथा इसके विकारों के रूप में कहा गया है।
अतः हम देखते हैं कि 'क्षेत्र' शब्द से अपरा प्रकृति की समस्त क्रिया-व्यवहार अभिप्रेत है। वह संपूर्ण क्रिया-व्यवहार यहाँ हमारी अन्तःस्थित देहधारी आत्मा का कर्मक्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसका वह बोध प्राप्त करती है। प्रकृतिजन्य यह समस्त जगत् अपनी मूल क्रिया में आध्यात्मिक दृष्टिबिन्दु के द्वारा जैसा दिखायी देता है उसका विविध और विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्राचीन द्रष्टा-ऋषियों, वेद और उपनिषदों के ऋषियों, के छंदों का संदर्भ दिया गया है जिनमें हम परमात्मा के द्वारा सृष्ट इन भुवनों का अंतःप्रेरित एवं अंतर्ज्ञानमय वर्णन पाते हैं, साथ ही इसके लिए हमें ब्रह्मसूत्रों की ओर भी निर्दिष्ट किया गया है जो हमें तार्किक एवं दार्शनिक विश्लेषण प्रदान करते हैं। गीता हमारी सत्ता की निम्नतर प्रकृति का सांख्य विचारकों की परिभाषा में संक्षिप्त व्यावहारिक वर्णन करके ही स्वयं को संतुष्ट कर लेती है। सबसे पहले आती है निर्विशेष अव्यक्त ऊर्जा; उसमें से पंच महाभूतों का बाह्य वस्तुनिष्ठ विकास हुआ; और इसके साथ ही इंद्रियों का, बुद्धि और अहंकार का आंतर आत्मनिष्ठ विकास हुआ; और साथ ही, इंद्रियों के पाँच विषय भी हैं, या यों कहें कि जगत् के इन्द्रिय बोध के पाँच भिन्न प्रकार, वे शक्तियाँ जो वैश्व-ऊर्जा ने अपने मूल बाह्य वस्तुनिष्ठ तत्त्व के द्वारा धारण की हुई पाँच मूलभूत स्थितियों से निर्मित नाना रूपों के पदार्थों से व्यवहार करने के लिए विकसित की हैं, – वे ऐंद्रियक संबंध जिनके द्वारा बुद्धि और इंद्रियों से संपन्न अहंकार जगत् की रचनाओं पर क्रिया करता है: यही क्षेत्र का स्वरूप है। फिर, एक सामान्य चेतना है जो ऊर्जा को उसके कार्यों में पहले तो अनुप्राणित करती और फिर उसे आलोकित करती है; उस चेतना की एक क्षमता (faculty) है जिसके द्वारा ऊर्जा पदार्थों के संबंधों को इकट्ठे धारण करती है; साथ ही, अपने विषयों के साथ हमारी चेतना के अंतर्बाह्य संबंधों की निरंतरता और दृढ़ता भी है। ये क्षेत्र की आवश्यक शक्तियाँ हैं; ये सब एक ही साथ मानसिक, प्राणिक और भौतिक प्रकृति की सर्वसामान्य और सार्वभौमिक शक्तियाँ भी हैं। सुख और दुःख, राग और द्वेष क्षेत्र के प्रधान विकार हैं। वेदांतिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि सुख और दुःख प्राणिक या संवेदनात्मक विकृतियाँ हैं जो निम्नतर शक्ति की क्रियाओं के संपर्क में आने पर आत्मा के सहज आनन्द पर लग जाती हैं। और इसी दृष्टिबिंदु से हम कह सकते हैं कि राग और द्वेष तदनुरूप मानसिक विकृतियाँ हैं जो निम्नतर शक्ति के द्वारा आत्मा के उस प्रतिक्रियात्मक संकल्प को प्रदान की जाती हैं जो इस ऊर्जा के संपकों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया निर्धारित करता है। ये सुख-दुःखादि द्वंद्व सकारात्मक और नकारात्मक भाव हैं जिनमें निम्नतर प्रकृति का अहंमय जीव संसार का उपभोग करता है। नकारात्मक भाव - वेदना, घृणा, दुःख, जुगुप्सा इत्यादि - विकृत या फिर अधिक-से-अधिक अज्ञानी रूप से विपरीत प्रतिक्रियाएँ हैं : सकारात्मक रूप – राग, सुख, हर्ष, आकर्षण - कुनिर्देशित प्रतिक्रियाएँ हैं, अथवा अपने अच्छे-से-अच्छे रूप में भी, ये अपर्याप्त हैं तथा सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की प्रतिक्रियाओं से हीन कोटि की हैं।
ये सब चीजें मिलकर इस प्राकृत जगत् के साथ हमारे प्रथम व्यवहारों का मूलभूत स्वरूप हैं, परंतु स्पष्ट ही यह हमारी सत्ता का संपूर्ण विवरण नहीं है; यह हमारा वर्तमान स्वरूप है पर हमारी संभावनाओं की सीमा नहीं। इससे परे भी कोई ज्ञेय वस्तु है, 'ज्ञेयम्', और जब क्षेत्रज्ञ स्वयं इस क्षेत्र के पीछे जो कुछ भी है उस सबको जानने के लिए अंतर्मुख होता है, अपने अंदर की ओर मुड़ता है तभी वास्तविक ज्ञान, 'ज्ञानम्' ज्ञाता का तथा क्षेत्र का सच्चा ज्ञान आरंभ होता है। एकमात्र वह अंतर्मुखता ही हमें अज्ञान से मुक्त करती है। क्योंकि, जितना अधिक हम अंदर जाते हैं, उतना ही अधिक पदार्थों की महत्तर तथा पूर्णतर यथार्थताओं को समझते हैं और ईश्वर एवं जीव तथा जगत् एवं उसकी क्रियाओं दोनों के पूर्ण सत्य को पकड़ पाते हैं। इसलिये, दिव्य गुरु कहते हैं कि क्षेत्र और उसके ज्ञाता दोनों का एक साथ ज्ञान ही, 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम्', संयुक्त और यहाँ तक कि एकीकृत आत्मज्ञान तथा विश्व-ज्ञान ही वास्तविक ज्ञानोद्दीपन और एकमात्र प्रज्ञा है। क्योंकि, आत्मा और प्रकृति दोनों ही ब्रह्म हैं, किंतु प्राकृत जगत् के वास्तविक सत्य को तो केवल उस मुक्त ज्ञानी द्वारा ही खोजा सकता है जिसे आत्मा का सत्य भी ज्ञात हो। एक ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति के अंदर विद्यमान एक यथार्थता ही समस्त ज्ञान का विषय है।
हम जितना अधिक अपनी गहराइयों में जाते जायेंगे उतनी ही अधिक भव्यताएँ हमें गोचर होती जाएँगी और इन गहराइयों का कोई अंत नहीं है। हमारे आध्यात्मिक साहित्य में जिन किन्हीं भी ऊँचे से ऊँचे लोकों का निरूपण हुआ है या कभी हो सकता है, वे सभी क्षेत्र हैं। क्षेत्रज्ञ स्वयं परमात्मा हैं।
प्रश्न : जब कहा जाता है कि 'अंतर्मुख होओ' तब किसे अंतर्मुख होने को कहा जाता है?
उत्तर : बाह्य सतही चेतना, जो हम अपने आप को प्रायः मानते हैं, उसे अंतर्मुख होना होता है। और जब वह अंतर्मुखीन होगी तब उसे अधिक विशालतर क्षेत्र गोचर होगा। सतही चेतना में सीमित और संकीर्ण क्षेत्र गोचर होता है। जैसे-जैसे हम भीतर अधिक गहराई में जायेंगे या ऊर्ध्वमुख आरोहण करेंगे वैसे-वैसे चीजों का एक अधिक गहरी और उच्चतर चेतना से अनुभव होगा जो चीजों के अधिक गहन सत्यों को हमारे समक्ष प्रकट करता है और हमें अधिक विशाल क्षेत्र का ज्ञान होता है। और इस आंतरिक और ऊर्ध्वमुख गति का कोई अंत नहीं है और ज्यों-ज्यों यह गति चलती रहती है त्यों-त्यों भागवत् चेतना को अपने आप को अधिकाधिक प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। वास्तव में तो सभी कुछ चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। चेतना की जैसी स्थिति होगी, वैसी ही सृष्टि हमें गोचर होगी। यदि ऐसा न होता और कोई नियत निर्धारित सृष्टि ही होती तब तो फिर चेतना के भेद से भी सृष्टि वैसी की वैसी ही दिखाई देनी चाहिये थी। परंतु किसी भी संवेदनशील और कुछ संस्कारित व्यक्ति को भली-भाँति इसका बोध होता है कि किस प्रकार चेतना के परिवर्तन के साथ ही साथ संपूर्ण दृश्य ही बदलता जाता है।
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ।। ८।।
८. अभिमान और दंभ का न रहना, अहिंसा, क्षमा, स्पष्टवादिता, (मन और शरीर की) शुचिता, दृढ़ता और स्थिरता, आत्म-संयम और आचार्य की उपासना।
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ।। ९।।
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। १० ।।
९-१०. इन्द्रियों के विषयों के प्रति अनासक्ति, अहंभाव का अभाव, जन्य, मृत्यु, वृद्धावस्था और दुःख के दोष का बोध होना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि के प्रति आसक्ति और ममत्व के भाव का अभाव, और समस्त प्रिय और अप्रिय घटनाओं के मध्य सतत् समचित्तता ।
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।। ११ ।।
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।। १२ ।।
११-१२. अनन्य योग के द्वारा मेरे प्रति अविचल भक्ति, निर्जन स्थान में निवास और मनुष्यों के समूहों तथा सम्मेलनों के प्रति रुचि का अभाव, आध्यात्मिक ज्ञान और तत्त्व ज्ञान के यथार्थ अर्थ का प्रत्यक्ष दर्शन, इसे ही ज्ञान कहा गया है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है।
इसके बाद गीता हमें बताती है कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, या यों कहें कि वह हमें यह बताती है कि ज्ञान की शर्तें क्या हैं, तथा उस मनुष्य के लक्षण एवं चिह्न क्या हैं जिसकी आत्मा आंतरिक ज्ञान अथवा प्रज्ञा की ओर मुड़ी होती है।.... सबसे पहला लक्षण है एक विशेष प्रकार की नैतिक अवस्था, प्राकृत सत्ता का सात्त्विक संचालन।.... इसके बाद उसमें होता है पूर्ण अनासक्ति और समता का एक अधिक उदात्त और अधिक मुक्त भाव, इंद्रियों के विषयों के प्रति होनेवाले प्राकृत सत्ता के आकर्षण से दृढ़ विरक्ति और सामान्य मानव को उत्पीड़ित करनेवाली उस अनवरत कोलाहलपूर्ण अहं-बोध, अहंभाव तथा अहं-प्रेरणा की माँगों से आमूल मुक्ति।... अंत में, जो वस्तुएँ वास्तव में महत्त्वपूर्ण हैं उनकी ओर होता है एक तीव्र अंतर्मुख झुकाव, अस्तित्व के सच्चे अभिप्राय तथा व्यापक तत्त्वों का दार्शनिक अनुभव, आंतरिक आध्यात्मिक ज्ञान और ज्योति की शांत निरंतरता, अविचल भक्तियोग, ईश्वर-प्रेम और विश्वव्यापी एवं सनातन उपस्थिति के प्रति हृदय की प्रगाढ़ और अखण्ड आराधना।
जब हम परमात्मा की ओर चलते हैं तब उसके सहज परिणामों के रूप में हमारे अंदर समता, अहंकार से मुक्ति आदि चीजें विकसित होती हैं। सामान्यतया समता, अहंकार से मुक्ति, इंद्रियों के संयमन आदि को हम उद्देश्य मान बैठते हैं जबकि अपने आप में ये भगवान् की ओर चलने के परिणाम हैं। भ्रमित होकर व्यक्ति इन्हीं को उद्देश्य मान बैठता है और इन्हें प्राप्त करने का प्रयास भी करता है परंतु इससे उसे प्रायः निराशा ही हाथ लगती है। अतः करने योग्य काम केवल यह है कि अनन्य रूप से परमात्मा की ओर गति की जाए और उन्हीं के निर्णय के ऊपर यह छोड़ दिया जाए कि वे हमारे अंदर जिस चीज को जिस मात्रा में विकसित करना चाहें वैसे करें। यदि उन्हें हमारे अहंकार से प्रयोजन हो तो इसका कोई कारण नहीं कि क्यों हमें अहंकार से मुक्त होने की चेष्टा करनी चाहिये। इसलिए सच्चे रूप से तो भगवान् स्वयं ही तय करेंगे कि हमारे अंदर की कौनसी चीज को विकसित करना है, किसे परिष्कृत करना है और किसका निर्मूलन करना है।
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते ।
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।। १३।।
१३. जिसे जानना है और जिसे जानकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है उसका अब मैं वर्णन करता हूँ; वह (ज्ञेय) आदि से रहित परं ब्रह्म है; उसे न सत् कहा जाता है न असत्।
परात्पर निरपेक्ष ब्रह्म की चेतना तथा वैयक्तिक एवं वैश्व सत्ता पर पड़नेवाले उसके प्रभाव के प्रति सचेतन होना ही चरम तथा सनातन ज्ञान है। हमारे मन-बुद्धि विभिन्न धाराओं से इस ज्ञान का विवेचन कर सकते हैं, इसके आधार पर विरोधी दर्शनों की रचना कर सकते हैं, इसे सीमित, संशोधित कर सकते हैं, इसके किन्हीं पहलुओं पर बहुत ही अधिक बल दे सकते हैं और दूसरों पर बहुत कम, इससे यथार्थ या त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं; परन्तु हमारे बौद्धिक विभेदों और अपूर्ण निरूपणों से इस चरम तथ्य में कोई अंतर नहीं पड़ता कि यदि हम विचार और अनुभव को इनकी पराकाष्ठा तक ले जाएँ तो जिस ज्ञान में ये परिसमाप्त होंगे वह यही है। अध्यात्म-ज्ञान के योग का लक्ष्य इस शाश्वत सद्वस्तु, इस आत्मा, इस ब्रह्म, इस परात्पर के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता जो सबके ऊपर और अन्दर अवस्थित है तथा जो व्यक्ति में अभिव्यक्त होता हुआ भी छिपा हुआ है, विश्व में प्रकट होकर भी प्रच्छन्न है.. ...जिसमें एकाग्र होने से हमारी तमसाच्छन्न तथा प्रकृति के कुहासे से परिवेष्टित अंतरात्मा अपनी अमर और परात्पर सहज मूल चेतना को पुनः प्राप्त करके उसका उपभोग करती है।
[सत् और असत्] चरम विप्रतिषेध (antinomy) हैं जिनके मध्य से कि हम अज्ञेय की ओर झाँकते है।... समस्त विप्रतिषेध एक-दूसरे का आमना-सामना करते हैं ताकि वे अपने विरोधी पहलुओं में विद्यमान एकमेव सत्य को पहचान लें और संघर्ष के तरीके से दोनों के भीतर के आपसी ऐक्य को ग्रहण कर सकें। ब्रह्म ही आदि और अन्त है। ब्रह्म ही एकमेव तत्त्व है जिसके अतिरिक्त और कुछ भी अस्तित्वमान नहीं है।
परन्तु यह ऐक्य अपने स्वरूप में अनिर्वचनीय है। जब हम इसे मन के द्वारा विचार में लाने का प्रयत्न करते हैं तो हमें अवधारणाओं और अनुभवों की अनन्त श्रृंखलाओं में से होकर चलना होता है। और फिर भी अन्त में हम अपनी विशालतम अवधारणाओं और अपने व्यापकतम अनुभवों को भी नकारने के लिए बाध्य होते हैं ताकि इस चीज की अभिपुष्टि कर सकें कि परम यथार्थता समस्त परिभाषाओं या वर्णनों से परे है। हम भारतीय ऋषियों के इस सूत्र पर पहुँचते हैं कि 'वह' यह नहीं है, 'वह' वह नहीं है, नेति नेतिः ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है जिससे हम 'उसे' सीमित कर सकते हैं, कोई भी ऐसी अवधारणा नहीं है कि जिससे उसे परिभाषित किया जा सके।
चरम विप्रतिषेध (antinomy) तो यही है कि परमात्मा अस्तित्वमान हैं भी और नहीं भी। ज्यों ही मानसिक रूप से हम उनके स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास करते हैं त्यों ही उसका विपरीत भी उतना ही सही हो जाता है ताकि परमात्मा किसी एक सूत्र में न बंध जाएँ। और परमात्मा दोनों विपर्ययों में होते हुए भी दोनों से परे होते हैं। वे एक-अनेक, वैयक्तिक-निर्वैयक्तिक, सचेतन-अचेतन, सर्वज्ञ-अज्ञानी आदि सभी रूपों में अभिव्यक्त होते हुए भी इन सभी से परे रहते हैं।
____________________
* अज्ञेय के द्वारा अपने-आप को विश्व-अस्तित्व के स्वतंत्र आधार के रूप में सिद्ध करना ही शुद्ध सत् है। इसके विपरीत 'उसकी' समस्त विश्व-अस्तित्व से मुक्तावस्था को हम असत् की संज्ञा देते हैं, - अर्थात् वास्तविक अस्तित्व के उन सभी प्रत्यक्ष रूपों से स्वतंत्रता जो विश्वगत चेतना अपने-आप के लिए निरूपित करती है, यहाँ तक कि अत्यंत अमूर्त रूपों से, अत्यंत विश्वातीत रूपों से भी स्वतंत्रता। अज्ञेय उन्हें अपने-आप को यथार्थ अभिव्यक्ति मानने से मनाही नहीं करता, परंतु वह सभी अभिव्यक्ति से अथवा किसी भी अभिव्यक्ति से अपने-आप को सीमित करना अस्वीकार करता है। जिस प्रकार शान्त-निश्चलता सक्रियता को व्यक्त होने देती है इसी प्रकार असत् सत् को व्यक्त होने देता है। इस साथ-साथ चलते निषेध और अभिपुष्टि के द्वारा, जो कि सभी विपरीत तत्त्वों की तरह ही एक-दूसरे के विनाशक न होकर पूरक हैं, प्रबुद्ध मनुष्य के लिए साथ-ही-साथ यह अनुभूति प्राप्त करना संभव हो जाता है कि जिस प्रकार चेतन आत्म-सत् एक यथार्थ तत्त्व है वैसे ही सर्वातीत अज्ञेय भी वही यथार्थ तत्त्व है।
'वे' हैं भी और नहीं भी हैं, और साथ ही होने और न होने से परे भी हैं। इसीलिए हमारे पुराण उनका वर्णन करते हुए 'नेति, नेति' और 'इति, इति' दोनों ही तरीकों से उनका स्वरूप बताते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमात्मा से उद्भूत न हुई हो और जिसमें वे स्वयं अभिव्यक्त न होते हों और फिर भी वे उससे परे रहते हैं। इन सब विपर्ययों और उनके समन्वय के माध्यम से इतना अवश्य है कि हमारी बुद्धि कुछ अधिक नमनीय हो जाती है जिससे कि जिस अतिशयता में गिरने की वह भूल करती थी उससे कुछ बचने की संभावना बन जाती है क्योंकि उसे यह भान हो जाता है कि परमात्मा हमारी किन्हीं भी परिभाषाओं से सर्वथा परे हैं।
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। १४।।
१४. उस (ब्रह्म तत्त्व) के हाथ और पैर सब ओर हैं, उसके नेत्र, सिर और मुख सभी ओर हैं, उसके कान सर्वत्र हैं, वह इस लोक में सबको ढककर (हमारे सब ओर व्याप्त होकर) स्थित है।
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ।। १५।।
१५. वह इन्द्रियों से रहित होकर भी समस्त इन्द्रियों और उनके गुणों में प्रतिबिंबित या आभासित होता है; अनासक्त होते हुए भी सभी कुछ का धारक है; समस्त गुणों से परे होकर भी गुणों का भोक्ता है।
बहिरन्तश्व भूतानामचरं चरमेव च ।
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ।। १६ ।।
१६. समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर है, चर-अचर *, दूरस्थ तथा अत्यंत समीप ये सब एक ही साथ 'वही' है; वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने के कारण हमारे ज्ञान से अतीत है।
हमारे मन का जैसा गठन है उसमें अपने अहंकार के कारण उसे यह बात कदाचित् ही समझ में आती है कि परमात्मा हमारी किन्ती से परिभाषाओं की पकड़ में नहीं आ सकते, वे हमारे किन्हीं भी मानसिक निरूपणों से सर्वथा परे हैं। हम यह तो सरलता से देख और समझ पाते है कि पाशविक चेतना मानवीय चेतना की क्रिया को नहीं समझ सकती, परंतु इसी बात को अपने अहं के कारण हम स्वयं अपने ऊपर लागू करने से चूक जाते हैं कि मानवीय चेतना भी भागवत् चेतना को समझ नहीं सकती। गीता में ही इससे पूर्व के एक अध्याय में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि किस प्रकार भगवान् सभी रूपों में हैं भी और नहीं भी हैं और साथ ही इन सब रूपों से सर्वथा परे भी हैं। इस सब का इतना लाभ अवश्य है कि हमारी बुद्धि अतिशय रूप से अपने पूर्वाग्रहों से लिप्त न रहकर कुछ अधिक नमनीय हो जाती है।
पुरुष और प्रकृति के सभी संबंध ब्रह्म की नित्यता के अंदर घटनाएँ हैं इन संबंधों के दर्पण और घटक के रूप में इन्द्रियाँ और गुण इन परम् पुरुष को उन क्रियाओं के प्रस्तुतिकरण के साधन हैं जो वस्तुओं में उनकी अपनी ही शक्ति निरंतर क्रियाशीलता में मुक्त करती रहती है। वे स्वयं इंद्रियों की सीमाओं से परे हैं,
___________________________
* हमें यह स्मरण रखना होगा कि स्थितिशीलता और गति, निरपेक्ष के विषय में उसी प्रकार हमारे मानसिक निरूपण मात्र हैं, जिस प्रकार एकत्व और बहुत्व हैं। निरपेक्ष स्थितिशीलता और गति दोनों से परे है, जैसे कि वह एकत्व और बहुत्व से परे है। परन्तु वह एक और स्थितिशील में शाश्वत रूप से प्रतिष्ठित रहता है और गतिशील और बहु में अनंत, अचिंत्य एवं सुनिश्चित रूप से अपने-आप के चक्कर काटता रहता है। विश्व-अस्तित्व शिव का एक ऐसा आनंदमय नृत्य है जो ईश्वर की देह को हमारी दृष्टि के सामने असंख्यगुणा बढ़ाता है; इस नृत्य के होते हुए भी वह निर्विकार शुद्ध सत् जहाँ था वहीं और जैसा था वैसा ही, जो कुछ सदा से है और रहेगा ठीक वही बना रहता है; इस विश्व-नृत्य का एकमात्र परम उद्देश्य है नृत्य का आनंद।
[परम तत्त्व] न सत् है न ही असत्; न संभूति है न असंभूति; न सगुण है न निर्गुणः न चैतन्य है न जड़; न पुरुष है न प्रकृति, न आनन्द है न निरानन्दः न मनुष्य है, न देवता और न ही पशु; 'वह' इन सब चीजों से परे है, वह जगत् के रूप में सभी चीजों को थामे रखता है और समाहित रखता है; वह ही ये सब चीजें है और वही ये सब चीजें बनता है।
वे सब वस्तुओं को देखते हैं पर स्थूल आँखों से नहीं, सब बातों को सुनते हैं पर स्थूल कर्णों से नहीं, सब वस्तुओं के विषय में सचेत अथवा अभिज्ञ हैं, किन्तु सीमित करने वाले मन से नहीं - मन तो केवल निरूपित करता है पर वास्तव में जान नहीं सकता। किन्हीं भी गुणों द्वारा निर्धारित न होते हुए, वे अपने तत्त्व में सब गुणों को धारण तथा उनका निर्धारण करते हैं और अपनी ही प्रकृति की इस गुणात्मक क्रिया का उपभोग करते हैं। वे जो कुछ करते हैं उसमें किसी के साथ भी आसक्त नहीं हैं, किसी से बद्ध नहीं हैं, किसी के भी अंदर लिप्त या मोहित नहीं हैं; शांत-स्थिर होते हुए वे अपनी विश्व-व्यापिनी शक्ति के समस्त कर्म, प्रयास और आवेग को विशाल तथा अमर स्वातन्त्र्य के साथ धारण करते हैं।
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।। १७।।
१७. वह प्राणियों में अविभक्त होते हुए भी विभक्त प्रतीत होता है। वह जो सृष्टिकर्ता, धर्ता और प्राणियों को प्रसने वाला है, वह ज्ञेय है।
सीमित को अविभक्त के एक विभाग के रूप में देखा जाता है, परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है: क्योंकि यह विभाग केवल दिखने में ही है, एक सीमा-निर्धारण तो होता है परन्तु कोई वास्तविक पार्थक्य सम्भव नहीं है। जब हम किसी वृक्ष या अन्य किसी पदार्थ को स्थूल आँखों से न देख कर आंतरिक दृष्टि और आन्तरिक इंद्रियबोध से देखते हैं तो जिस तत्त्व के विषय में हम सचेत होते हैं वह उस वृक्ष या उस पदार्थ का संघटन करने वाला एक अनन्त अखण्ड सत्-तत्त्व होता है जो उसके प्रत्येक परमाणु और अणु में व्याप्त होता है, जो अपने-आप में से उनकी रचना करता है, जो सम्पूर्ण प्रकृति का, सम्भूति की प्रक्रिया का, अन्तःस्थ ऊर्जा की क्रिया का निर्माण करता है; ये सभी चीजें वही है, ये सभी यह अनन्त, यह सत्-तत्त्व ही हैः हम उसे इस रूप में देखते हैं कि वह अविभक्त रूप से बने रहते हुए अपना विस्तार करता है और समस्त पदार्थों को एकीभूत करता है जिससे कि कोई भी पदार्थ यथार्थ में उससे पृथक् नहीं है और न दूसरे पदार्थों से पृथक् है। गीता कहती है कि "वह भूतों में अविभक्त है और फिर भी ऐसे स्थित है मानो विभक्त हो।" इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ वही अनन्त है और अन्य सभी पदार्थों के साथ भी, जो कि उस अनन्त के ही नाम, रूप और शक्तियाँ हैं, सार तत्त्व में एक है।
समस्त विभागों और विभिन्नताओं में यह अदम्य ऐक्य अनन्त का गणित है जिसका संकेत उपनिषद् के इस वचन में किया गया है: - "यह पूर्ण है और वह पूर्ण है; पूर्ण में से पूर्ण घटाने पर पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है।"
ब्रह्म के लिये कोई पूर्ण और अंश नहीं होते, अपितु प्रत्येक पदार्थ ही स्वयं पूर्ण है और ब्रह्म के पूर्णत्व से लाभान्वित होता है।...यह अविभक्त है और सौर-मंडल एवं चीटियों की बांबी को एक साथ ही न केवल अपना समान ही अंश अपितु अपना संपूर्ण स्वत्व दे देता है।
जब परमात्मा के स्वरूप का ऐसा वर्णन होता है कि अखिल ब्रह्माण्ड भी उनकी सत्ता के कण मात्र के बराबर है तो व्यक्ति कल्पना करता है कि परमात्मा इससे अनंत रूप से विशाल और महान् होंगे। परंतु इसके साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि एक छोटे से छोटे कण में भी परमात्मा पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं। कहने का अर्थ है कि किसी बालू के कण में भी परमात्मा उतने ही पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं जितने पूर्ण रूप से वे असंख्यों ब्रह्माण्डों में व्याप्त रहते हैं। यही आत्मा की गणित है। 'पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। - यह ऐसी गणित है जहाँ यह भी पूर्ण है और वह भी पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण को निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है। यह किसी सीमित चीज की गणित नहीं अपितु अनंत की गणित है। इसलिए परमात्मा को अन्यत्र कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे अपने अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हैं।
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ।। १८ ।।
१८. वह, समस्त ज्योतियों की परम ज्योति, अन्धकार से परे कहा जाता है: वह ज्ञान द्वारा प्राप्त होनेवाला ज्ञेय है और ज्ञानगम्य है, सभी के हृदयों में स्थित है।
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ।। १९।।
१९. इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप में बता दिये गये हैं। इस प्रकार जानते हुए मेरा भक्त मेरे भाव को, मेरी सत्ता की प्रकृति और पद को प्राप्त होता है।
[इसलिए, यह जानना] सत्य की महज कोई बौद्धिक परिकल्पना या स्पष्ट पहचान ही नहीं है, न वह हमारी सत्ता के विभिन्न प्रकारों का कोई आलोकित मनोवैज्ञानिक अनुभव ही है। यह एक 'साक्षात्कार' या 'उपलब्धि' है, इस शब्द के पूर्ण अर्थ में; यह परमात्मा, परात्पर तथा विश्वगत भगवान् का हमारे लिये और हमारे अन्दर साक्षात्कार कर लेना, उन्हें यथार्थ बना लेना है, और उसके बाद यह असंभव हो जाता है कि हम सत्ता के विभिन्न प्रकारों को उस परम् आत्मा के प्रकाश में तथा उनके सच्चे स्वरूप में उन्हें हमारे जगत्-अस्तित्व की मनोवैज्ञानिक और भौतिक अवस्थाओं के बीच आत्मा की सम्भूति (becoming) के प्रवाह के रूप में न देखकर किसी अन्य रूप में देखें। इस उपलब्धि में तीन क्रमिक क्रियाएँ हैं, आंतरिक दृष्टि, पूर्ण आन्तरिक अनुभव और तादात्म्य - [मेरी प्रकृति और पद, मद्भावं, की उपलब्धि ।।
यह आंतरिक दृष्टि, एक ऐसी शक्ति जिसे प्राचीन ऋषियों द्वारा इतना अधिक मूल्य दिया जाता था, एक ऐसी शक्ति जो किसी मनुष्य को पहले की तरह निरा विचारक न छोड़कर ऋषि या कवि बना देती थी, अन्तरात्मा के अन्दर एक प्रकार का ऐसा प्रकाश है जिसके द्वारा अदृष्ट वस्तुएँ इसके लिये केवल बुद्धि के लिये ही नहीं, अपितु आत्मा के लिये भी - उतनी ही प्रत्यक्ष और वास्तविक हो जाती हैं जैसी कि दृष्ट वस्तुएँ स्थूल आँख के लिये होती हैं। भौतिक जगत् में ज्ञान के सदा ही दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष का तात्पर्य है उस वस्तु का ज्ञान जो आँखों के सामने हो और परोक्ष का तात्पर्य है उस वस्तु का ज्ञान जो हमारी दृष्टि से दूर और परे हो। जब वस्तु हमारी दृष्टि से परे हो तो हम आवश्यक रूप से उसके विषय में अनुमान, कल्पना एवं उपमान या तुल्यता (analogy) के द्वारा, जो दूसरे लोग उसे देख चुके हैं उनके वर्णनों को सुनकर अथवा यदि उपलब्ध हों तो उसके चित्रात्मक या अन्यविध निरूपणों का अध्ययन करके ही उसके बारे में किसी धारणा पर पहुँचने के लिये बाध्य होते हैं। इन सब साधनों को एक साथ प्रयुक्त करके हम अवश्य ही उस वस्तु के विषय में किसी न्यूनाधिक सटीक धारणा पर या उसकी किसी सांकेतिक प्रतिमा पर पहुँच सकते हैं, परन्तु स्वयं उस वस्तु की हमें अनुभूति नहीं होती; वह अभी तक हमारे लिये कोई ऐसी यथार्थता नहीं होती जिसे ग्रहण किया या समझा जा चुका हो, अपितु किसी यथार्थता का केवल हमारा वैचारिक या धारणात्मक निरूपणमात्र होती है। परन्तु एक बार जब हमने उसे आँखों से देख लिया होता है- क्योंकि और कोई भी इन्द्रिय पर्याप्त नहीं है, - तो हम उसे अधिकृत और उपलब्ध अथवा अनुभूत कर लेते हैं; वह वहाँ हमारी तृप्त सत्ता में सुनिश्चित-सुरक्षित होती है, हमारा ज्ञानगत अंग होती है। आंतरात्मिक चीजों के संबंध में और आत्मा के संबंध में भी ठीक यही नियम लागू होता है। भले हम दार्शनिकों या गुरुओं से अथवा प्राचीन ग्रन्थों से आत्मा के विषय में स्पष्ट और प्रकाशपूर्ण उपदेश सुन लें; भले हम विचार, अनुमान, कल्पना, उपमान या अन्य किसी उपलब्ध साधन के द्वारा इसकी मानसिक आकृति बनाने या मानसिक परिकल्पना करने का यत्न भी कर लें; भले ही हम उस परिकल्पना को अपने मन में दृढ़तापूर्वक धारण कर लें और एक समग्र एवं अनन्य एकाग्रता के द्वारा उसे अपने अन्दर जमा भी लें; किन्तु हमने अभी तक आत्मा को उपलब्ध नहीं किया है, हमने ईश्वर के दर्शन नहीं किये हैं। जब सुदीर्घ और निरंतर एकाग्रता के बाद या अन्य साधनों के द्वारा मन का आवरण विदीर्ण या दूर कर दिया जाता है, जब प्रबुद्ध अथवा जागृत मन के ऊपर ज्योति का प्रवाह, ज्योतिर्मय ब्रह्म, फूट पड़ता है और परिकल्पना एक ऐसी ज्ञान-दृष्टि को स्थान दे देती है जिसमें आत्मा वैसा ही प्रत्यक्ष, वास्तविक और मूर्त होता है जैसी कि स्थूल वस्तु नेत्र के लिये होती है, केवल तभी हम ज्ञान में उसे उपलब्ध करते हैं; क्योंकि तब हमने दर्शन कर लिये होते हैं। उस दर्शन के बाद प्रकाश के क्षीण होने के चाहे कितने ही काल, अन्धकार के चाहे कितने ही अन्तराल आत्मा को पीड़ित क्यों न करें, यह जिस वस्तु को एक बार अधिकृत कर चुकी है उसे इस प्रकार से कभी नहीं खो सकती कि पुनः प्राप्त ही न कर सके। अनुभव अनिवार्य रूप से नवीनीकृत होता रहता है और निश्चय ही और भी अधिक नियमित रूप से होने लगता है जब तक कि वह स्थायी ही नहीं हो जाता; ऐसा कब और कितने कम समय में होता है यह उस भक्ति एवं दृढ़ता पर निर्भर करता है जिसके साथ हम मार्ग पर डटे रहते हैं और गुप्त भगवान् को अपने संकल्प या प्रेम के द्वारा घेर लेते हैं।
__________________
* ज्ञान योग की त्रिविध कार्यप्रणाली का यही भाव है - श्रवण, मनन, निदिध्यासन।
यह आन्तरिक दृष्टि मनोवैज्ञानिक अनुभव का एक प्रकार है; किन्तु आन्तरिक अनुभव उस दृष्टि तक ही सीमित नहीं है; दृष्टि केवल उद्घाटित करती है, वह आत्मा का आलिंगन नहीं करती। ठीक उसी प्रकार जैसे आँख को, यद्यपि वह अकेली ही साक्षात्कार का प्रथम आभास ले आने में सक्षम होती है, सर्वालिंगनकारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले स्पर्श तथा अन्य ज्ञानेंद्रियों के अनुभव की सहायता को बुलाना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मा के अन्तर्दर्शन को भी हमें अपने सभी अंगों में इसके अनुभव के द्वारा पूर्ण बनाना चाहिये। हमारी सम्पूर्ण सत्ता को, न कि केवल हमारी आलोकित ज्ञान-दृष्टि को ही, भगवान् की माँग करनी चाहिये। क्योंकि, चूँकि हमारे अंदर प्रत्येक तत्त्व आत्मा की एक अभिव्यक्ति मात्र है इसलिये प्रत्येक पुनः अपनी यथार्थता तक पहुँच सकता तथा उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकता है। हम आत्मा का एक मानसिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और उन सब ऊपरी तौर पर अमूर्त वस्तुओं को - चेतना, शक्ति, आनन्द और इनके नानाविध रूपों एवं क्रियाओं को - जो मन के लिये सत्ता का स्वरूप है, ठोस यथार्थताओं के रूप में ग्रहण कर सकते हैं: इस प्रकार मन ईश्वर के विषय में संतृप्त हो जाता है। 'प्रेम' और हृद्गत आनन्द के द्वारा, - अपनी अन्तःस्थित आत्मा एवं विश्वगत आत्मा के द्वारा, तथा जिनके भी साथ हमारे सम्बन्ध हैं उन सब में स्थित आत्मा के प्रेम एवं आनन्द के द्वारा - हम आत्मा की भावात्मक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं: इस प्रकार हृदय ईश्वर के विषय में संतृप्त हो जाता है। सौन्दर्य में हम आत्मा की एक सौंदर्यबोधी या रसात्मक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं तथा उस परम यथार्थता का, जो हमारे द्वारा या प्रकृति के द्वारा सृष्ट सभी कुछ के भीतर सौंदर्यबोधी मन तथा इन्द्रियों के प्रति अपने आकर्षण में सर्व-सुन्दर है, आनन्द-बोध तथा रसास्वादन प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार इन्द्रियाँ ईश्वर के विषय में संतृप्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि समस्त जीवन एवं रचना में तथा उन शक्तियों, बलों एवं सामर्थ्यो की, जो हमारे या दूसरों के द्वारा या जगत् में क्रिया करते हैं, सभी क्रियाओं में भी हम आत्मा का प्राणिक एवं स्नायविक अनुभव और लगभग भौतिक अनुभव या संवेदन भी प्राप्त कर सकते हैं: इस प्रकार प्राण और शरीर भी ईश्वर के विषय में संतृप्त हो जाते हैं।
भगवान् का अनुभव केवल दृष्टि तक ही सीमित नहीं होता। उनका अनुभव हम अपनी सभी इन्द्रियों के माध्यम से, यहाँ तक कि रोम-रोम में कर सकते हैं। हमारी सभी इन्द्रियों का औचित्य ही यही है कि वे अपने-अपने तरीके से भगवान् का साक्षात्कार या अनुभव प्राप्त कर सकें। श्रीअरविन्द के अनुसार अतिमानसिक सत्ता में भी अपने प्रकार की इंद्रियाँ होंगी जिनका अनुभव या संवेदन प्राप्त करने का अपना ही विशेष तरीका होगा। अतिमानस से ऊपर के स्तर पर भी संभवतः अपने प्रकार की इंद्रियाँ होती होंगी जो परमात्मा को अपने विशिष्ट तरीके से अनुभव करती होंगी।
यह सब ज्ञान और अनुभव तादात्म्य पर पहुँचने तथा उसे अधिकृत करने के प्राथमिक साधन हैं। वह हमारी अपनी ही आत्मा है जिसका हम साक्षात्कार और अनुभव करते हैं और इसलिये वह साक्षात्कार और अनुभव तब तक अपूर्ण ही रहते हैं जब तक कि वे तादात्म्य में परिणत नहीं हो जाते और जब तक हम अपनी समस्त सत्ता में परम वेदान्तिक ज्ञान 'मैं वही हूँ (सोऽहमस्मि)' को चरितार्थ करने में समर्थ नहीं हो जाते। हमें ईश्वर का केवल साक्षात्कार और आलिंगन ही नहीं करना होगा, अपितु वही सत्-तत्त्व बन जाना होगा।
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि ।
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ।। २० ।।
२०. प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जान; और तू यह भी जान कि विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं।
कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।। २१ ।।
२१. प्रकृति कार्य, कारण और कर्त्तापन के भाव की उत्पत्ति का कारण कही गयी है; पुरुष सुख और दुःखों के भोग का कारण (अर्थात् भोक्ता) कहा गया है।
पुरुष और प्रकृति शाश्वत ब्रह्म के दो पहलू मात्र हैं, यह एक ऊपरी रूप से देखने में द्वैत है जो उनकी विश्वमय सत्ता की क्रियाप्रणालियों को आधारित करता है। पुरुष अनादि और शाश्वत है, प्रकृति भी अनादि और शाश्वत है। परंतु प्रकृति के गुण और जो निम्नतर रूप वह हमारे सचेतन अनुभव में धारण करती है, उन गुणों और रूपों की उत्पत्ति इन दो सत्ताओं के पारस्परिक आदान-प्रदान से होती है। वह सब कुछ जो यहाँ अनित्य और क्षरणशील या परिवर्तनशील है, वे सब रूप प्रकृति से उद्भूत होते हैं, उसी के द्वारा वे कार्य और कारण, कर्म और कर्मफल, शक्ति और उसकी क्रिया की श्रृंखला को अपने ऊपर ले लेते हैं। वे निरंतर ही बदलते रहते हैं और उनके साथ ही पुरुष और प्रकृति भी बदलते प्रतीत होते हैं, परंतु अपने-आप में ये दो शक्तियाँ शाश्वत तथा सदा समान रहती हैं। प्रकृति सृजन और क्रिया करती है, पुरुष उसकी सृष्टि और कर्म का उपभोग करता है; किन्तु अपने कर्म के इस निम्नतर रूप में वह इस उपभोग को सुख-दुःख के तमोमय और क्षुद्र रूपों में बदल देती है।
प्रश्न : इस अध्याय के ही सातवें श्लोक में भगवान् कहते हैं कि 'इच्छा' या कामना क्षेत्र का ही लक्षण है। जबकि पहले हमने चर्चा की थी कि श्रीअरविन्द के अनुसार कामना और अहंकार तो आत्मपरक अर्थात् पुरुष पक्ष की ग्रंथियाँ हैं और द्वंद्व और गुण प्रकृति पक्ष की ग्रंथियाँ हैं। एक स्थान पर तो कामना को प्रकृति की ग्रंथि बताते हैं और दूसरे स्थान पर उसे पुरुष पक्ष की ग्रंथि बताते हैं, तो यह विरोधाभास कैसे?
उत्तर : कामना का मूल उद्गम पुरुष ही है। पुरुष के अंदर जो संकल्प होता है वही जब प्रकृति पक्ष के पास आता है तब वह विकृत होकर कामना का रूप ले लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि पुरुष त्रिगुणों से ऊपर होकर ईश्वर भाव में स्थित होता है तब तो उसे त्रिगुणों की बाध्यता नहीं होती, परंतु जब तक उसे त्रिगुण प्रभावित करते हैं तब तक उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वह मुक्त रूप से अपने संकल्प को अभिव्यक्त कर सके और इसलिए जब उसका संकल्प अभिव्यक्ति में आता है तब वह कामना का रूप ले लेता है। अतः कामना आत्मनिष्ठ चीज है न कि वस्तुनिष्ठ। इस अध्याय के सातवें श्लोक में कामना को क्षेत्र का लक्षण नहीं बतलाया गया है, केवल उसके परिणामों सुख और दुःख - - को ही ऐसा बतलाया गया है।
प्रश्न : सातवें श्लोक में भगवान् कहते हैं, 'अव्यक्त (मूल प्रकृति), पंच महाभूत, दस इंद्रियाँ और एक मन, बुद्धि और अहंकार, तथा पाँच इंद्रियों के विषय (तन्मात्रा); राग और द्वेष, सुख और दुःख, संघात, चेतना और धृति (दृढ़ता), इन सब को मिलाकर क्षेत्र तथा इसके विकारों के रूप में कहा गया है।' तब फिर क्षेत्र का अर्थ क्या प्रकृति से है?
उत्तर : हाँ, परंतु एक दूसरे दृष्टिकोण से, जब गीता कहती है कि 'पराप्रकृतिर्जीवभूता', तो इसका यह भी अर्थ है कि जितने भी पुरुष हैं वे परमेश्वर के नहीं अपितु पराप्रकृति के ही रूप हैं। सभी कुछ केवल पराप्रकृति माँ जगदम्बा की ही अभिव्यक्ति है। जिस किसी भी तत्त्व का हमें आज तक कोई भी ऊँचे से ऊँचा, गहन से गहन अनुभव भी प्राप्त हुआ है या कभी हो सकता है, वह सब केवल पराप्रकृति का ही रूप है। परम तत्त्व तो केवल एक ऐसी उपस्थिति मात्र है जो पराप्रकृति की क्रिया पर अपनी सहमति की छाप लगाती है और उसे किसी भी प्रकार न तो जाना जा सकता है और न ही उसका अनुभव किया जा सकता है।
और वास्तव में तो परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए भगवान् स्वयं ही साक्षी पुरुष हैं और स्वयं अपने ही तत्त्व का साक्षित्व कर रहे हैं। अतः जिस तत्त्व को वे देखते हैं उसे हम पराप्रकृति की संज्ञा देते हैं और स्वयं उन्हें हम साक्षी पुरुष, अथवा ईश्वर या अन्य कई संज्ञाएँ देते हैं। यही चीज जब पार्थिव अभिव्यक्ति में आती है तब पराप्रकृति के द्वारा ही मनोमय, प्राणमय आदि पुरुषों की और स्वयं ईश्वर की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक कि अतिमानसिक ईश्वर भी पराप्रकृति से ही अभिव्यक्त होता है। अतः इस दृष्टिकोण से तो पराप्रकृति के अतिरिक्त वास्तव में और कुछ है ही नहीं।
वर्तमान प्रसंग में हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिये कि पुरुष और प्रकृति के परस्पर आदान-प्रदान से किस प्रकार गुणों की उत्पत्ति होती है। प्रायः हम अपने ग्रंथों में ऐसा उल्लेख पाते हैं कि देवता सात्त्विक होते हैं, असुर राजसिक होते हैं और पिशाच आदि तामसिक होते हैं। देवताओं में अन्य कोई गुण नहीं होते। वहीं अतिमानस में तो किन्हीं गुणों की विद्यमानता ही नहीं होती, वह तीनों गुणों से परे है। पराप्रकृति जब इस पार्थिव अभिव्यक्ति में आती है तब चेतना का अवतरण पामसक से प्राणिक और प्राणिक से जड़भौतिक तत्व तक होता है। केवल मानव ही ऐसी सत्ता है जिसमें ये तीनों ही स्तर क्रियारत हैं जिसके कारण उसकी प्रकृति त्रिगुणमय होती है। बुद्धि प्रधानतः सात्त्विक होती है, प्राण राजसिक और भौतिक देह तामसिक। हालाँकि किसी एक गुण की प्रधानता होने पर भी इन तीनों भागों में भी समय-समय पर अन्य गुणों का भी प्रभाव पड़ता रहता है। उदाहरण के लिए सत्त्वप्रधान होने पर भी बुद्धि के अंदर प्राण तथा देह के कारण राजसिक और तामसिक गुणों का प्रवेश और बाहुल्य होता रहता है। इसी प्रकार तीनों भागों में परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया चलती रहती है। चूंकि मानव सत्ता से प्राण और देह को अलग नहीं किया जा सकता इसलिए भले ही मन सत्त्व प्रधान हो तो भी देह की तामस् प्रकृति और प्राण की राजस् प्रकृति अवश्य ही उस पर अपना प्रभाव डालती हैं और इन दोनों पर भी मन की सात्त्विक क्रिया होती है। भौतिक देह में भी प्राण के संचार के साथ रजस् और सत्त्व का प्रभाव होता रहता है। इसलिए प्रत्येक भाग में अपने-अपने गुण की प्रधानता अवश्य होती है परंतु एकांगी रूप से कोई गुण विद्यमान नहीं होता। इन तीनों गुणों को हम पुरुष-प्रकृति की परस्पर क्रिया के तीन भाव या उसकी तीन स्थितियाँ कह सकते हैं। तामसिक गुण में पुरुष लगभग पूरी तरह प्रकृति के अधीन होता है, वह प्रकृति की क्रिया से बाध्य होता है। ऐसी स्थिति में पुरुष को प्रकृति की आदतों की मर्यादाओं के अनुसार चलना होता है। जब प्राण का प्रवेश होता है तब भी पुरुष प्रकृति की आदतों से छूट तो नहीं निकल सकता परंतु उसे अपनी क्रिया करने का अधिक स्थान मिल जाता है। इसीलिए राजसिकता आने पर व्यक्ति तामसिक अवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक मुक्त रूप से क्रिया कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राण पर जड़भौतिक प्रकृति के नियम बाध्यकारी नहीं होते। प्राणिक प्रकृति के नियम अधिक नमनीय हैं इसीलिए उसके प्रभाव से राजसिक अवस्था में व्यक्ति घोर कर्म भी कर सकता है जबकि तामसिक अवस्था में तो किसी प्रकार की क्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा आदि ही नहीं प्राप्त होती। अतः प्राणिक स्तर पर पुरुष को प्रकृति के साथ आदान-प्रदान में कुछ अधिक स्वतंत्रता होती है और वह प्रकृति के ऊपर तामसिक अवस्था की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र रूप से क्रिया कर सकता है। सात्त्विक अवस्था में पुरुष की स्वतंत्रता इससे भी अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में पुरुष तामसिक और राजसिक अवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक मुक्त रूप से प्राणिक और भौतिक प्रकृति पर अपनी क्रिया कर सकता है। इसी कारण हम देखते हैं कि जिनमें मानसिकता सच्चे रूप में विकसित होती है वे अपने शरीर और प्राण पर अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक संयम और नियंत्रण रख पाते हैं और उनकी अपेक्षा कहीं अधिक उदात्त अभिव्यक्ति भी कर पाते हैं। इसी प्रकार चेतना का आरोहण करते हुए जब हम अतिमानसिक स्तर पर पहुँचते हैं वहाँ पुरुष और प्रकृति समस्थिति में होते हैं। उस स्थिति में पुरुष के ऊपर प्रकृति की किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रहती। प्रकृति की बाध्यता के कारण निचले स्तरों पर जो कुछ करना संभव नहीं था वह इस स्तर पर संभव हो जाता है। इसीलिए निचले स्तर पर जो तीन गुण थे वे अब नहीं रहते। अतिमानसिक स्तर से और ऊपर जाने पर प्रकृति पूर्णतः पुरुष के अधीनस्थ होती है और स्वयं ही पुरुष की प्रसन्नता के अनुसार सभी कुछ की व्यवस्था करती है। परंतु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि इस अभिव्यक्ति के अंदर हम जिस पुरुष और प्रकृति की बात कर रहे हैं वे पराप्रकृति के ही रूप हैं, उसी की क्रीड़ा के अंग हैं। जिन परम पुरुष की हम बात करते हैं वे ये निम्न पुरुष नहीं हैं। परम पुरुष तो एक ऐसी सूक्ष्मातिसूक्ष्म उपस्थिति है जो हमारे किन्हीं भी अनुभवों से परे है परंतु फिर भी जो पूर्ण रूप से सर्वत्र और सर्वदा ही विद्यमान है। वह उपस्थिति, या भगवान् की वह कृपा तो सभी कुछ को धारण करती है, सभी कुछ को अवलंब प्रदान करती है। उस उपस्थिति को हम परम पुरुष कह सकते हैं। और जो भी क्रिया-कलाप हमें गोचर होता है, या जिसका हमें अपनी गहरी से गहरी स्थिति में अनुभव हुआ है या भविष्य में कभी हो सकता है वह सब माँ जगदंबा की, पराप्रकृति की क्रिया है। वास्तव में परम पुरुष और परा प्रकृति में कोई तात्त्विक भेद नहीं है। परंतु इस निम्न प्रकृति में पुरुष और प्रकृति में तीन विभाजन हो जाते हैं जिनकी परस्पर क्रिया से तीन गुण बन जाते हैं। इनकी क्रिया के साथ ही साथ अहं की क्रिया के कारण इच्छा उत्पन्न होती है। बिना अहं के इच्छा नहीं हो सकती। और उस इच्छा की पूर्ति या अभाव पर हमारा सुख-दुःख निर्भर करता है। यदि अहं न हो तब तो एकत्व की चेतना होगी। अहं ही 'मैं' और 'दूसरे' का बोध प्रदान करता है और जैसे ही अपने से अलग सत्ताओं का बोध आता है वैसे ही परस्पर आदान-प्रदान का, अभाव की पूर्ति करने का भाव आता है, इच्छा उठती है। एक पृथक् सत्ता के पीछे औचित्य यह है कि वह भगवान् के एक विशिष्ट पहलू की अभिव्यक्ति के लिए होती है। कोई भी दो सत्ताएँ एक समान अभिव्यक्ति नहीं कर सकती और वास्तव में तो किसी एक ही अभिव्यक्ति को या पहलू को दोहराने का कोई अर्थ भी नहीं है। इस पृथक्ता के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपने-अपने तरीके की इच्छा उठती है। आरंभ में यह इच्छा भौतिक आवेगों के रूप में, काम-क्रोधादि आवेगों के रूप में प्रकट होती है, उसके बाद यह कुछ अधिक परिष्कृत कामनाओं - अपनी पद-प्रतिष्ठा, आत्म-गौरव आदि भावों – के रूप में प्रकट होती है, और उसके बाद नैतिक आदशों, विचारों आदि भावों की अधिक विशालतर तुष्टि के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार यह एक अधिकाधिक परिष्कृत होती अभिव्यक्ति है जिसमें प्रकृति-पुरुष का परस्पर आदान-प्रदान चलता रहता है जिसमें पुरुष को जितनी ही अधिक स्वतंत्रता होती है उतना ही अधिक वह प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाता है। और प्रत्येक सत्ता क्या विशिष्ट अभिव्यक्ति करेगी यह योजना पराप्रकृति द्वारा निहित की जाती है इसलिए बाहरी रूप से व्यक्ति भले किसी भी प्रकार के कर्मों, इच्छाओं, कामनाओं, आवेगों, विचारों, भावों आदि में क्यों न लिप्त हो, परंतु अंततः गति उसको उस विशिष्ट अभिव्यक्ति की ओर होती है जिसे पराप्रकृति ने उसके अंदर निहित किया है। गीता भी इन्हीं गुणों से आरोहण कर के गुणों से परे जाने की बात करती है। परंतु आरोहण का यह मार्ग बड़ा ही विकट है इसलिए भगवान् कहते हैं कि उनके प्रति भक्ति के द्वारा व्यक्ति अधिक सहजता से यह आरोहण कर सकता है। अर्जुन को वे उपदेश करते हैं कि 'अक्षर ब्रह्म तीनों गुणों से परे है इसलिए उसी की शरण में जा'। परंतु ऐसा कहकर वे कहते हैं कि 'अक्षर ब्रह्म का आधार 'मैं' स्वयं हूँ अतः मेरी शरण में आ जा'। अतः भक्ति के द्वारा व्यक्ति निस्त्रैगुण्य की स्थिति में जा सकता है।
अब प्रश्न उठता है कि जब भगवान् के अनंत गुण हैं तब फिर उन्हें केवल तीन ही गुणों में क्यों बाँध दिया गया है। तो ऐसा इसलिए है कि इस पार्थिव अभिव्यक्ति में मन-प्राण-शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त करने के कारण उन सभी गुणों पर इन हिस्सों की छाप लग जाती है और वे गुण भी हमें सत्त्व, रज और तम के तीन विभाजनों के अंतर्गत ही दिखाई देने लगते हैं। हालाँकि यह भी देखने और समझाने का एक दृष्टिकोण मात्र ही है क्योंकि वास्तविक क्रिया तो माँ भगवती की हो रही है जो हमारे किन्हीं भी वर्णनों से सर्वथा परे है। माँ भगवती अपनी क्रिया में स्वतंत्र हैं। उन पर हमारी कोई भी परिभाषाएँ, हमारे कोई भी नियम-विधान, पुरुष-प्रकृति आदि की हमारी धारणाएँ लागू नहीं होतीं। वे तो भगवान् को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करती हैं। परंतु जिस रूप में वे भगवान् के गुणों की अभिव्यक्ति करती हैं वह मन-प्राण-देहमय सत्ता होने के कारण हमारी दृष्टि को त्रिगुणमयी प्रतीत होती है।
जब हम कहते हैं कि सब कुछ माँ भगवती की ही इच्छा से अभिव्यक्त होता है और उन्हीं का संकल्प अमोघ रूप से प्रभावी होता है तब फिर उसमें हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं-कामनाओं आदि की क्या भूमिका है? जब हम इसे कुछ-कुछ समझ जाएँगे तो हम हमारे चित्त, अवचेतन आदि भागों की क्रियाओं को भी कुछ अधिक बेहतर रूप में समझ पाएँगे। हमारे चित्त और अवचेतन में हमारे अपने सभी जन्मों के संस्कार, मनुष्यजाति की सभी धारणाएँ, हमारी सभी पाशविक प्रवृत्तियाँ, भय आदि संचित हैं। इसमें वह सब कुछ संचित होता है जिसके विषय में हम अपने वर्तमान या अतीत जीवनों में सचेतन थे या नहीं थे। हमारे मन के विचार, आँखों के सामने से गुजरा कोई दृश्य, कोई गंध, या शब्द या स्पर्श सभी कुछ इसके भंडार में संचित रहते हैं। वह सब भी संचित रहता है जो हमने कभी भी अपनी सूक्ष्म इंद्रियों से महसूस किया हो। इस सब को मिलाकर हमारे पास सूचना का एक अतिविशाल भंडार बन जाता है। अतः जब तक व्यक्ति इतना पर्याप्त विकसित नहीं होता कि माँ भगवती के संकल्प को सचेतन रूप से पहचान सके और सचेतन रूप से उसके अनुसार क्रिया कर सके, तब तक वह संकल्प आता तो अपने मूल स्रोत माँ भगवती से ही है परंतु बिना हमारे उसके विषय में सचेतन हुए वह हमारे मन आदि के द्वारा हमारे चित्त और अवचेतन भागों में चला जाता है और वहाँ से अपनी पूर्ति के लिए आवश्यक अभीप्साओं, सूचनाओं, उत्प्रेरणाओं, आवेगों-प्रवेगों, कामनाओं, लालसाओं, क्रोधों, भयों आदि अनेकानेक तरीके के भावों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार वह संकल्प आकर हमारे इन भागों में वे आवश्यक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर देता है जो उसकी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। इसलिए भले ही हमें वे इच्छाएँ आदि सभी भाव हमारे अपने अंदर उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे माँ भगवती की क्रिया के ही परिणाम हैं और इस परोक्ष प्रक्रिया को वह इसलिए काम में लेती है क्योंकि अभी तक हम उसकी किया के विषय में सचेतन नहीं होते। वास्तव में साधना और कुछ नहीं केवल उस क्रिया के प्रति सचेतन होना है ताकि उसमें हम सचेतन रूप से भाग ले सकें, जिससे कि हमारे अंदर उनकी क्रिया अधिक त्वरित हो सके और उसकी अभिव्यक्ति के आनंद में हम सहभागी हो सकें।
परंतु भले प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से, जब माँ भगवती की ही इच्छा कार्यान्वित होती है तब फिर क्रमविकास का तथा उत्तरोत्तर पूर्णता का क्या स्थान है? एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति के पास कोई कर्मचारी है जो बहुत लोभी और लालची है। व्यक्ति उसके स्वभाव को भली-भाँति जानता है इसलिए अपना काम पूरा करा सके उसके लिए वह उसके स्वभाव के माध्यम से उससे काम कराता है। अपना काम कराने के लिए वह उसके साथ प्रलोभन, डाँट-डपट आदि सभी आवश्यक तरीके काम में लेता है। अतः अंततः कर्मचारी काम तो वही करता है जो कि मालिक चाहता है परंतु इसके लिए मालिक को अनेक टेढ़ी रीतियाँ काम में लेनी पड़ती हैं। वहीं यदि कर्मचारी बहुत समर्पित भाव से काम करता हो तब तो उसके इन परोक्ष तरीकों को काम में लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती क्योंकि वह तो मालिक की इच्छा को भली-भाँति क्रियान्वित करता है। और यदि वफादार होने के साथ ही साथ वह बहुत अधिक कुशल भी हो तब तो फिर मालिक के आदेश को और अधिक श्रेष्ठ रूप से पूर्ण कर सकेगा। इस प्रकार यह उत्तरोत्तर बढ़ती पूर्णता है। जितनी ही अधिक पूर्णत्व की अवस्था में वह कर्मचारी होगा उतने ही श्रेष्ठ रूप से वह अपने मालिक की इच्छा को क्रियान्वित कर सकेगा। साधना ठीक यही काम करती है। वह व्यक्ति को विकसित और सुसंस्कृत बनाकर भगवान् के संकल्प के प्रति संवेदनशील बना देती है ताकि सचेतन रूप से वह उसे समझ कर उसे क्रियान्वित कर सके। जब व्यक्ति पर्याप्त रूप से भगवद् संकल्प के प्रति खुला होता है तब अपनी अभिव्यक्ति के लिए उस संकल्प को किन्हीं परोक्ष रीतियों की आवश्यकता नहीं रहती और वह सीधे ही साधक के अंदर काम करने लगती है। पृथ्वी पर जो भी महान् या विशिष्ट कार्य हम अतीत या वर्तमान में होता देखते हैं वे सदा ही तब संभव हो पाते हैं जब निम्न क्रिया की बजाय भागवत् संकल्प को मानव माध्यम के द्वारा सीधे ही अभिव्यक्त होने का अवसर प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति सच्चे रूप से भागवत् संकल्प के प्रति समर्पित हो तो मन, प्राण और शरीर के कोलाहलों से भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। इसलिए संभव है कि साधक ऐसा कार्य कर जाए या ऐसे किसी अभियान का बीड़ा उठा ले जिसे स्वयं उसकी बाहरी प्रकृति न समझती हो, या जिसे वह अस्वीकार करती हो, यहाँ तक कि जिसके परिणामों से अर्जुन की भाँति थर्राती हो। अपनी पुस्तक 'ऐसेज डिवाइन एण्ड ह्यूमन' में श्रीअरविन्द एक स्थान पर कुछ इस प्रकार कहते हैं कि 'जब मैं बोलने को होता हूँ तो बुद्धि सोचती है कि मैं अमुक बात कहूँगी, और तभी भगवान् मुँह से मेरे वे शब्द तो ले लेते हैं और मेरे होठ कुछ और ही कह उठते हैं जिससे बुद्धि थर्रा उठती है।* यह एक ऐसी स्थिति है जो बिना अनुभव हुए केवल मानसिक रूप से नहीं समझी जा सकती। और यह अनुभव केवल तभी आ सकता है जब भीतर से कोई चीज भगवद् संकल्प के प्रति इतनी समर्पित हो कि वह हमारी बाहरी प्रकृति की कुछ भी परवाह किये बिना मुक्त रूप से हमारे द्वारा अपनी क्रिया करता है। अतः ज्यों-ज्यों व्यक्ति भगवान् के प्रति अधिकाधिक समर्पित होता जाएगा त्यों ही त्यों भगवान् का अधिकाधिक महत्तर सत्य और अद्भुत भव्यताएँ अभिव्यक्त हो पाएँगी। यदि यंत्र निष्ठावान् नहीं है तब तो फिर वही गुणों की क्रिया चलती रहती है और अधिक से अधिक केवल निम्न मानवीय अभिव्यक्ति ही हो पाएगी, ऐसे में किसी दिव्य अभिव्यक्ति की कोई अधिक संभावना नहीं रहती। इसी अधिकाधिक दिव्य अभिव्यक्ति के लिए क्रमविकास चल रहा है। अब जिस प्रकार पाशविक चेतना की सीमितता के कारण एक स्तर से अधिक की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार मानव चेतना की सीमितता के कारण प्रकृति एक उच्चतर सत्ता को धरती पर लाने में प्रयासरत है जिसे श्रीअरविन्द अतिमानसिक सत्ता का नाम देते हैं और वे कहते हैं कि वस्तुओं की स्वाभाविक गति में अतिमानसिक चेतना का आविर्भाव एक अवश्यंभावी चीज है जिसे कोई टाल नहीं सकता। भले ही हमारे जड़भौतिक तत्त्व के रूपांतरण की बात वर्तमान में एक कपोलकल्पना या एक सर्वथा बेतुकी बात लगती हो, परंतु मानव के आविर्भाव से पूर्व कदाचित् बंदरों को भी मनुष्य के आने का कोई अंदेशा नहीं था। अतः श्रीमाताजी व श्री अरविन्द ने न केवल उस चेतना के अवतरण की घोषणा की, बल्कि जीवनपर्यंत उसे उतार लाने का प्रयास किया और उसका अवतरण संभव बनाया। जब वह चेतना प्रकट रूप से पृथ्वी पर अभिव्यक्त होगी तभी भागवत् साम्राज्य स्थापित होगा। सूक्ष्म स्तर पर वह चेतना कार्यरत है और जो कोई उसके प्रति अभीप्सा रखता है और उसके प्रति खुला है उसे अवश्य ही उस चेतना की क्रिया का कुछ अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए करने का केवल एक hat sigma' कार्य है कि किसी भी प्रकार उस चेतना के प्रति अपने आप को खोलना ताकि वह हमारे अंदर और हमारे द्वारा अधिकाधिक अपनी क्रिया संसिद्ध कर पाए।
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।। २२।।
२२. प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों का भोग करता है; गुणों में आसक्ति ही अच्छी और बुरी योनियों में उसके जन्म का कारण होती है।
किसी रूप या आकार के अंदर विद्यमान व्यष्टिगत आत्मा या सचेतन सत्ता अपने-आप को इस अनुभव करने वाले पुरुष के साथ या इस क्रियाशील प्रकृति के साथ तदाकार कर सकती है। यदि वह अपने-आप को प्रकृति के साथ तदाकार करती है तो वह स्वामी, भोक्ता और ज्ञाता नहीं होती अपितु प्रकृति की क्रियाओं के गुणों को प्रतिबिंबित करती है। अपनी इस तदाकारता से वह उस अधीनता और यांत्रिक क्रिया-प्रणाली में भाग लेती है जो इस प्रकृति का अपना विशेष लक्षण है। यहाँ तक कि प्रकृति में पूर्णतया लोन होकर यह आत्मा अचेतन या अवचेतन बन जाती है, प्रकृति के स्थूल रूपों में पूर्ण रूप से प्रसुप्त हो जाती है जैसे मिट्टी और धातु में, या फिर लगभग प्रसुप्त हो जाती है जैसे वनस्पति-जीवन में। वहाँ, उस अचेतना में, वह तमस् के प्रभुत्व के अधीन होती है।....(इस अवस्था से और अधिक आगे) पाशविक प्रकृति गठित और विकसित होती है जो चेतना में संकीर्ण, बुद्धि में अल्पविकसित या बिल्कुल प्रारंभिक तथा प्राणिक आदत और आवेग में राजस-तामसिक होती है। घोर अचेतना से एक आध्यात्मिक पद की ओर और भी अधिक ऊपर उठकर देहधारी पुरुष सत्त्व को, अर्थात् प्रकाश के गुणा को, उन्मुक्त करता है और कुछ-कुछ स्वतंत्रता, स्वामित्व तथा ज्ञान प्राप्त करता है और इसके साथ ही आन्तरिक सन्तोष और प्रसन्नता का सीमित तथा मर्यादित बोध प्राप्त होता है। स्थूल देह में मनोमय पुरुष वाले मनुष्य के प्रकृति ऐसी ही होनी चाहिए, परन्तु इन कोटि-कोटि देहधारी जीवों में से कुछ एक को छोड़कर किसी की भी प्रकृति ऐसी नहीं होती। सामान्यतः उसमें अन्धकारमय पार्थिव जड़ता और बेचैन अज्ञ पाशविक जीवन-शक्ति इतनी अधिक होती है कि वह प्रकाशमय और आनन्दमय आत्मा या फिर एक समस्वर संकल्प और ज्ञान से युक्त मन भी नहीं बन सकता। इस अवस्था में मनुष्य के अंदर स्वतन्त्र, ईश्वर, ज्ञाता और भोक्ता पुरुष के सच्चे स्वरूप की और आरोहण अपूर्ण, और अभी तक विघ्न-बाधा और विफलता से ही आक्रान्त रहता है। क्योंकि, मानवीय और पार्थिव अनुभव में ये (सत्त्व, रज और तम) सापेक्ष गुण हैं; इनमें से कोई भी अपना ऐकान्तिक और पूर्ण फल नहीं प्रदान करता; सभी एक-दूसरे से मिले हुए हैं और इनमें से किसी एक की भी शुद्ध क्रिया कहीं नहीं पायी जाती। इनकी अस्तव्यस्त और अनिश्चित परस्पर-क्रिया ही अहंकारमय मानव-चेतना, जो प्रकृति के अनिश्चित संतुलन में झूलती रहती है, के अनुभवों को निर्धारित करती है।
गुणों के विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं परंतु यहाँ श्रीअरविन्द ने गुणों तथा उनकी कार्य-प्रणाली को और अधिक प्रकाश में ला दिया है जिससे कि हम इस विषय को और अधिक गहराई से समझ सकते हैं।
प्रश्न : क्या हम कह सकते हैं कि सभी कुछ अन्तरात्मा पर ही टिका हुआ है?
उत्तर : इसके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो श्रीमाताजी ने एक संदर्भ में कहा था कि केवल चैत्य पुरुष को ही हमारे जीवन का संचालन करने का अधिकार है क्योंकि सच्चे स्वरूप में हम वही हैं। मन, प्राण और शरीर आदि तो ऊपरी वस्त्र मात्र हैं। अंतरात्मा हो हमारा वह सच्चा भाग है जो कि पूर्ण स्वतंत्र होता है और यह उसके चयन पर निर्भर करता है कि वह अपने आप को प्रकृति के साथ तदाकार करती है या पुरुष के साथ। इस स्वतंत्रता के कारण ही पुरुष भिन्न-भिन्न भाव अपना सकता है। जब वह साक्षी भाव अपनाता है तब वह गुणों की क्रिया को तटस्थ भाव से देख सकता है। यदि वह अक्षर पुरुष के भाव को अपनाता है तब उसमें क्षर प्रकृति की किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती, हालाँकि इसमें क्षर प्रकृति पर किसी प्रकार का कोई स्वामित्व नहीं होता। वह तो निम्न प्रकृति से अप्रभावित रहते हुए केवल उसका साक्षित्व कर सकता है। इस भाव में प्रकृति की उपेक्षा कर दी जाती है और उसे शांत होने के लिए अपने ही हाल पर छोड़ दिया दोला है। परंतु इस भाव में उपेक्षित रह जाने के कारण प्रकृति का देर जातपत्य स्पष्ट नहीं होता। क्योंकि इससे तो यह आभास होता है कि करने का केवल एक ही काम है और वह है किसी भी प्रकार इस प्रकर से छूट निकलना। परंतु गीता ऐसे किसी दृष्टिकोण को स्थान नहीं देती। गीतो इस समस्या का निराकरण पुरुषोत्तम की सत्ता के प्रतिपादन द्वारा करती है। गीता के अनुसार प्रकृति केवल पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के निमित्त ही कार्य करती है, न कि अक्षर पुरुष की प्रसन्नता के निमित्त। अतः, हमारी अंतरात्मा इसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है कि वह चाहे तो प्रकृति के साथ तदाकार हो सकती है और चाहे तो पुरुष के साथ। हमारी अंतरात्मा में ईश्वर के प्रति सहज आकर्षण होता है। यह क्रमविकासमय गति का अनुसरण करती है। परंतु हमारे अंदर भगवान् की अंतर्यामी उपस्थिति भी होती है जो क्रमविकासमय नहीं है। वह उपस्थिति निवर्तन (involution) से आती है। यह उपस्थिति स्वयं ईश्वर हैं जो हमारे हृदेश में विराजमान होते हैं। यही उपस्थिति सर्वत्र विद्यमान रहती है और सभी ब्रह्माण्डों और सभी लोकों का आधार है जो उन्हें धारण करती है, उन्हें अवलंब प्रदान करती है। पार्थिव जगत् क्रमविकासमय है क्योंकि इसमें चैत्य या अंतरात्मा निहित है। परंतु ऐसे भी लोक हैं या ऐसी भी अभिव्यक्तियाँ हैं जहाँ चैत्य विधान प्रभावी नहीं होता पंरतु फिर भी परमात्मा की उपस्थिति तो वहाँ भी विद्यमान रहती है। चैत्य या अंतरात्मा तो केवल पृथ्वी की ही विशिष्टता है। श्रीमाताजी के अनुसार अन्य लोकों में चैत्य पुरुष नहीं होता, इसलिए देवताओं को भी अपने विकास के लिए मानव शरीर धारण करना होता है।
हमारी अंतरात्मा, हमारी चैत्य सत्ता का स्वभाव ही है सहज रूप से भगवान् की ओर चलना। जब किसी साधक ने श्रीअरविन्द से कुछ इस प्रकार पूछा कि उसे चैत्य पुरुष के प्रति समर्पण करना चाहिये या फिर दिव्य शक्ति के प्रति या फिर श्रीमाँ के प्रति, तो इसके उत्तर में श्रीअरविन्द स्पष्ट रूप से कुछ इस प्रकार उत्तर देते हैं कि 'इस विषय में स्वयं को भ्रमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को दिव्य शक्ति के प्रति नहीं अपितु स्वयं श्रीमाँ के प्रति समर्पण करना चाहिये। और यदि चैत्य पुरुष स्वयं अभिव्यक्त होता है तो वह भी स्वयं अपने लिए समर्पण की माँग नहीं करेगा अपितु श्रीमाँ के प्रति समर्पण करने को ही कहेगा कि अतः हमारा चैत्य पुरुष अपने स्वभावमात्र में ही परम प्रभु के प्रति निष्ठावान् है, उनके प्रति समर्पित है। इसलिए उसके अंदर स्वयं अपने आप पर केंद्रित कोई भाव आ ही नहीं सकता। वह तो हर हालत में परम प्रभु पर ही केंद्रित रहता है। चैत्य पुरुष बना ही परमात्म तत्त्व से है इसलिए सहज ही उसमें अपने उद्गम के प्रति आकर्षण होता है। और चूंकि उसमें अपने उद्गम के प्रति आकर्षण होता है इसी कारण उसे क्रमविकास के साथ संलग्न कर दिया गया क्योंकि केवल उसी के आधार पर क्रमविकास हो सकता है। अन्य किसी भाग में अपने आप में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। अतः चैत्य के प्रभाव से ही हमारे अन्य सभी भाग धीरे-धीरे अपने मूल उद्गम के प्रति आकर्षित होते हैं और उसकी ओर गति करते हैं।
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ।। २३ ।।
२३. साक्षी, अनुमंता, भर्ता और भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा, इस देह में अवस्थित परम् पुरुष को इस प्रकार पुकारा जाता है।
पुरुष और प्रकृति के बीच गीता में किया गया भेद हमें उन विविध वृत्तियों का सूत्र दे देता है जो कि पुरुष पूर्ण स्वतंत्रता और प्रभुत्व की ओर अपनी गति में प्रकृति के प्रति अपना सकता है। गीता कहती है कि पुरुष साक्षी, भर्ता, अनुमन्ता, ज्ञाता, ईश्वर और भोक्ता है, प्रकृति (पुरुष के आदेश को) कार्यान्वित करती है, यह क्रियाशील तत्त्व है और पुरुष की वृत्ति के अनुरूप ही इसकी क्रिया होती है। पुरुष चाहे तो शुद्ध साक्षी का भाव अपना सकता है; वह प्रकृति के कार्य को एक ऐसी वस्तु के रूप में देख सकता है जिससे वह अलग खड़ा होता है; वह उसके कार्य का अवलोकन करता है, पर स्वयं उसमें भाग नहीं लेता। सब प्रवृत्तियों को शान्त करने की इस क्षमता का महत्त्व हम देख ही चुके हैं; यह पीछे हटने की या निवृत्ति की उस क्रिया का आधार है जिसके द्वारा हम प्रत्येक वस्तु के, - शरीर, प्राण, मानसिक क्रिया, विचार, संवेदन, भावावेश के, - सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि "यह प्रकृति है जो प्राण, मन और शरीर में कार्य कर रही है, यह स्वयं मैं नहीं हूँ, न ही यह मेरी चीज है" और इस प्रकार हम इन चीजों से पुरुष की पृथक्ता पर और इनकी शांत अवस्था पर पहुँचते हैं। साक्षी की वृत्ति अपने उच्चतम सप अनासक्ति का तथा जगज्जीवन की घटनाओं के प्रभाव से मुक्ति का चरम रुप होती है।
___________________
* CWSA 32, p. 147
प्रश्न : जब व्यक्ति साक्षी भाव अपना लेता है तब भी प्रकृति से तामसिक, राजसिक या सात्त्विक बनी रह सकती है?
उत्तर : जब तक व्यक्ति मन, प्राण और शरीर से संलग्न रहता है तब तक सच्चे रूप से साक्षी भाव नहीं आ सकता। यह स्थिति तो तब आती है जब व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान अक्षर पुरुष में स्थित होता है। अतः इस भाव में व्यक्ति अक्षर पुरुष की निर्लिप्तता आदि में भागीदार बन जाता है। क्षर पुरुष में यह चेतना नहीं हो सकती। जब तक व्यक्ति क्षर सत्ता अर्थात् अपने मन, प्राण और शरीर तथा इनकी क्रियाओं से बद्ध रहेगा तब तक वह सही साक्षी भाव नहीं अपना सकता। सारी समस्या तो हमारी संलग्नता के कारण आती है। अब यदि अमरीका में कोई कार दुर्घटना होती है तो हम उससे कदाचित् ही विचलित होने वाले हैं। पर यदि उस कार में हमारा कोई प्रिय व्यक्ति सवार होता तब फिर सारी भावनाओं आदि की उथल-पुथल शुरू हो जाएगी। अतः साक्षी भाव में व्यक्ति इन किन्हीं भी क्षर भागों से संलग्न नहीं होता। इसीलिए हमारी पारंपरिक योग पद्धतियों में पूरी तरह अक्षर पुरुष से तदात्म होकर निम्न प्रकृति को पूरी तरह से त्याग देने का उपाय बताया जाता रहा है। इस विषय में श्रीअरविन्द का कहना है कि किसी आत्मा विशेष के लिए तो यह मार्ग उचित हो सकता है परंतु सभी के लिए यह कोई उचित मार्ग नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो आत्मा का पार्थिव अभिव्यक्ति में आने का सारा हेतु ही निष्फल हो जाता है। अतः वे कहते हैं, "इस वैश्व चक्र का उद्देश्य यह नहीं कि वह यथाशीघ्र, उन स्वर्गों की ओर लौट जाये जहाँ पूर्ण प्रकाश और आनंद शाश्वत हैं या अतिवैश्व आनंद में जा पहुँचे, न ही इसका उद्देश्य है अज्ञान के लम्बे असंतोषजनक खाँचे में एक प्रयोजनहोन चक्कर लगाते रहना, उसमें ज्ञान की सतत् खोज करना और कभी उसे पूर्ण रूप से न पाना - उस अवस्था में अज्ञान सर्वचेतन की एक ऐसी मूल होगा जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती या फिर दुःखद और उद्देश्यहीन तथा समान रूप से अव्याख्येय आवश्यकता। इसका उद्देश्य है अतिवैश्व से भिन्न अवस्थाओं में, वैश्व सत्ता में आत्मा के आनंद को अनुभव करना और मूर्त रूप में जड़ सत्ता की अवस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोधों में भी आनंद और प्रकाश के स्वर्ग को पाना, अतः आत्मानुसंधान की ओर परिश्रम करना मानव शरीर में अंतरात्मा के जन्म का और अपने चक्रावर्तनों के क्रम में मानव जाति के श्रम का सच्चा प्रयोजन प्रतीत होता है। अज्ञान एक आवश्यकता है, यद्यपि है बहुत ही गौण, जिसे वैश्व ज्ञान ने अपने ऊपर आरोपित कर लिया है ताकि वह गति सम्भव हो सके जो बड़ी भूल या पतन नहीं अपितु सोद्देश्य अव तरण है, कोई अभिशाप नहीं, दिव्य अवसर है। सर्व-आनंद को पाना और उसे उसकी बहुविधता के तीव्र सार रूप में मूर्तिमान करना, ऐसे अनंत सत् की संभावना को प्राप्त करना जिसे अन्य अवस्थाओं में नहीं पाया जा सकता, जड़ पदार्थ में से भगवान् के मंदिर का निर्माण करना ही वह कार्य प्रतीत होता है जो जड़ भौतिक विश्व में जन्मी आत्मा को सौंपा गया है।" (CWSA 21. p. 613)
जब श्रीअरविन्द अलीपुर जेल में थे तब उनमें यही प्रश्न प्रबल रूप से उठा कि ब्रह्म जो पूर्ण, निरपेक्ष, अनंत है, जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई कामना नहीं वह अपने अंदर रूपों के इन जगतों का निर्माण करने के लिये चेतना की शक्ति को आखिर क्यों प्रक्षिप्त करता है? मनुष्य की तो अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहने की बाध्यता हो सकती है परंतु भगवान् की ऐसी कोई बाध्यता नहीं दिखाई देती कि क्यों उन्हें इस सीमितता, अज्ञान, अंधकार आदि में आकर फँसना पड़े। जब वे इसी विषय पर गहन चिंतन में थे तब उन्हें स्वामी विवेकानन्द का सम्पर्क सूक्ष्म जगत् में प्राप्त हुआ। इस विषय में श्रीअरविन्द के हो एक शिष्य ए.बी. पुराणी की पुस्तक 'द लाइफ ऑफ श्रीअरविन्द' में १० जुलाई १९२६ को हुई वार्ता में श्रीअरविन्द कहते हैं, "विवेकानन्द आए और उन्होंने मुझे अंतर्भासात्मक मानसिकता का ज्ञान प्रदान किया। उस समय तक मुझे उसका लेशमात्र भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने मुझे हर बिंदू को समझाते हुए विस्तार से ज्ञान प्रदान किया। यह संपर्क लगभग तीन सप्ताह तक चला और फिर वे अंतर्धान हो गए।"
इसी प्रकार का उल्लेख हमें उनके अन्य एक शिष्य नीरदवरन को पुस्तक 'टॉक्स विद श्री अरविन्द' के खण्ड एक, पृष्ठ १३८ पर एक वार्ता में मिलता है जहाँ श्रीअरविन्द कहते हैं कि, "उन्होंने (विवेकानंद जी ने) मुझे विस्तार से अतिमानस के कार्य के बारे में समझाया ठीक-ठीक अतिमानस के विषय में तो नहीं, अपितु अंतर्भासीकृत मन - जैसा कि वह अतिमानस के द्वारा सुव्यवस्थित होता विषय में बताया। 3 - 3 उन्होंने 'अतिमानस' शब्द का प्रयोग नहीं किया, यह नाम तो बाद में पैर दिया।"
स्वयं गीता के समय भी प्रचलित मानसिकता यही थी कि यह संसार अनित्य है और इससे किसी प्रकार पीछा छुटा लेना चाहिये। इसी लिए नवें अध्याय के तैंतीसवें श्लोक में भगवान् कहते हैं 'अनित्यममुत लोकमिमं । पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास में श्रीअरविन्द ही हैं जिन्होंने पहली बार पृथ्वी पर दिव्य जीवन के आविर्भाव का उद्घोष किया है और भौतिक शरीर तक के रूपांतर का दर्शन प्रदान किया है। हालाँकि वैदिक युग में भागवत् चरितार्थता का दर्शन था परंतु भौतिक रूपांतर का रहस्य तब तक उद्घाटित नहीं हुआ था। पहली बार श्रीअरविन्द ने ही इसकी घोषणा की है और इस रूपांतर को अवश्यंभावी और नियत बताया है।
शुद्ध साक्षी के रूप में पुरुष प्रकृति के भर्ता या धारक का कार्य करने से इन्कार कर देता है। भर्ता कोई और ही है, ईश्वर या शक्ति या माया, पर पुरुष नहीं।... जब तक सत्ता में एक स्पष्ट एवं वास्तविक द्वैत न हो, यह इस विषय का सम्पूर्ण सत्य नहीं हो सकता; पुरुष भर्ता भी है, वह अपनी सत्ता में उस शक्ति को धारण करता है जो विश्वरूपी दृश्य को प्रदर्शित करती है और जो इसकी शक्तियों का संचालन करती है। जब पुरुष भर्तापन को स्वीकार करता है, तब भी वह इसे निष्क्रिय रूप में तथा आसक्ति के बिना कर सकता है, यह अनुभव करते हुए कि वह शक्ति तो प्रदान करता है, पर ऐसा नहीं है कि वह इसका नियंत्रण एवं निर्धारण करता है। नियंत्रण करनेवाला कोई और ही है, ईश्वर या शक्ति या माया का निज स्वरूप.... परन्तु यदि (पुरुष द्वारा) भर्ता की वृत्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो समझना चाहिये कि सक्रिय ब्रह्म के साथ तथा उसकी विराट् सत्ता के आनन्द के साथ तादात्म्य की ओर उसने एक महत्त्वपूर्ण पग आगे बढ़ा लिया है.... क्योंकि जब पुरुष। भरण करने के लिये पूर्ण रूप से सहमत हो जाता है तो समझो कि अनुमति ने सक्रिय रूप धारण कर लिया है, चाहे पुरुष प्रकृति की सब शक्तियों को प्रतिबिम्बित तथा धारण करने के लिये और इस प्रकार उनकी क्रिया को बनाये रखने के लिये सहमत होने से अधिक कुछ भी न करे, अर्थात् शक्तियों के कार्य का निर्धारण और चुनाव न करे एवं यह माने कि स्वयं ईश्वर या शक्ति या कोई ज्ञानमय संकल्पशक्ति ही चुनाव और निर्धारण करती है.. परन्तु इसके सामने जो कार्य प्रस्तुत किये जायें उनमें से यदि यह सामान्यतः कुछ को पसंद करे तथा दूसरों का त्याग करे तो समझो कि यह उनका निर्धारण करने लगा है; जो बहुत कुछ निष्क्रिय था वह अब पूर्ण रूप से सक्रिय अनुमन्ता बन गया है और एक सक्रिय नियंता बनने की राह पर है।
पुरुष नियंता तब बनता है जब वह प्रकृति के ज्ञाता, ईश्वर और भोक्ता के रूप में अपना पूर्ण कार्य स्वीकार करता है। ज्ञाता के रूप में पुरुष उस शक्ति का ज्ञान रखता है जो क्रिया करती है और निर्धारण करती है, वह सत्ता के मूल्यों को देखता है जो विश्व में अपने आप को चरितार्थ कर रहे हैं, वह नियति के रहस्य में प्रवेश करता है। क्योंकि जो शक्ति कार्य करती है वह स्वयं भी ज्ञान के द्वारा निर्धारित होती है जो कि उसका उद्गम है तथा उसके मूल्यों का व उन मूल्यों के संपादन का स्रोत और निर्धारक है। इसलिए जिस अनुपात में पुरुष पुनः ज्ञाता बनता जाता है, वैसे ही वह क्रिया का नियंता भी बनता जाता है... और ऐसा वह सक्रिय भोक्ता बने बिना नहीं कर सकता। निम्नतर सत्ता में उपभोग द्विविध प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, जो कि इंद्रिय संवेदनों के विद्युत् प्रवाह में हर्ष और शोक का रूप धारण कर लेता है; परंतु उच्चतर सत्ता में यह आत्म-अभिव्यक्ति जनित दिव्य आनन्द का सक्रिय रूप से समान ही उपभोग होता है। इसमें स्वतंत्रता में कोई हानि नहीं होती, अज्ञानमय आसक्ति में कोई पतन नहीं होता। अपनी आत्मा में मुक्त मनुष्य को यह बोध होता है कि भगवान् ही प्रकृति के कर्म के स्वामी हैं, माया सभी कुछ को निर्धारित और कार्यान्वित करने वाली उनकी ज्ञानमय संकल्पशक्ति है, शक्ति इस द्विविध दिव्य शक्ति (माया) का संकल्पात्मक पक्ष है जिसमें ज्ञान सदा ही उपस्थित रहता है और अमोघ होता है; व्यक्तिगत रूप में भी पुरुष अपने आप के विषय में इस रूप में सचेत होता है कि दिव्य सत्ता का एक केंद्र है, - ईश्वर का अंश है... - और उतने अंश में वह प्रकृति के उस कर्म को नियंत्रित करता है जिसका वह अवलोकन, भरण, अनुमोदन, उपभोग करता है और जिसे वह जानता है और जिसे ज्ञान की निर्धारक शक्ति के द्वारा नियंत्रित करता है; और जब वह अपने आप को विश्वमय बना लेता है, तो उसका ज्ञान केवल दिव्य ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है, उसका संकल्प केवल दिव्य संकल्प को कार्यान्वित करता है, वह केवल दिव्य आनन्द का उपभोग करता है न कि किसी अज्ञानमय व्यक्तिगत संतुष्टि का। इस प्रकार पुरुष अपनी मुक्तावस्था को अपने अधिकार में सुरक्षित रखता है, विराट् पुरुष के एक प्रतिनिधि के रूप में विराट् अस्तित्व का उपभोग एवं आनन्द करता हुआ भी सीमित व्यक्तित्व के त्याग की अवस्था को सुरक्षित रखता है। उच्चतर स्थिति में उसने पुरुष और प्रकृति के सच्चे संबंधों को पूर्णरुप स्वीकार कर लिया होता है.... पुरुष का अपने आप में चरम आनन्द लेना उस पर आधारित पुरुष का प्रकृति में चरम आनन्द लेना ही इस संबंध की दिव्य परिपूर्णता है।
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ।। २४।॥
२४. जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष को और अपने गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, वह चाहे जैसे भी रहे या कर्म करे, वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता।
....प्रकृति पुरुष की ही क्रिया है, अपनी निज प्रकृति के द्वारा सचेतन पुरुष क्रियारत हैः अतः पुरुष और विश्व-ऊर्जा, शान्त-निश्चल आत्मन् और आत्मा की स्रष्ट्री शक्ति कोई यथार्थ में दोहरे और पृथक् तत्त्व नहीं हैं अपितु द्वयेक (biune) हैं। जैसे हम अग्नि और अग्नि की शक्ति को पृथक् नहीं कर सकते, वैसे ही, कहा जाता है कि, हम दिव्य सत्-तत्त्व और उसकी चित्-शाति को पृथक् नहीं कर सकते। आत्मा की इस रूप में प्रथम अनुभूति कि वह अत्यन्त प्रगाढ़ रूप से शान्त है और शुद्ध रूप से निष्क्रिय है, यह उसका सम्पूर्ण सत्य नहीं है।.... इस शरीर में आसीन हैं उसके (प्रकृति के) और हमारे भगवान्, परमात्मन्, परम् पुरुष, प्रकृति के महेश्वर, जो उसके कार्य का अवलोकन करते हैं, उसकी क्रियाओं का अनुमोदन करते हैं, वह जो कुछ करती है उसका भरण करते हैं, उसकी अनेकविध सृष्टि पर नियंत्रण अथवा शासन करते हैं, अपने सार्वभौम आनन्द के साथ अपनी ही सत्ता के प्रकृति द्वारा रचित रूपों की इस क्रीड़ा का उपभोग करते हैं। इससे पहले कि हम अपने आप को सच्चे रूप में शाश्वत का सनातन अंश जान सकें, यह वह आत्म-ज्ञान है जिससे हमें अपनी मानसिकता को सुपरिचित कराना होगा। एक बार जब वह आत्म-ज्ञान सुस्थिर हो जाये, तब चाहे हमारी अंतरात्मा प्रकृति के साथ अपने आदान-प्रदान में बाहरी तौर पर अपने आप को कैसे भी आचरणों में डाले, वह चाहे कुछ भी क्यों न करती दिखायी दे या वह व्यक्तित्व, सक्रिय शक्ति तथा देहबद्ध अहंभाव के चाहे जैसे इस या उस रूप को धारण करती हो क्यों न प्रतीत हो, फिर भी वह अपने-आप में स्वतंत्र होती है, पहले को तरह जन्मचक्र से आबद्ध नहीं रहती, क्योंकि वह आत्मा की निर्व्यक्तिकता में सत्ता मात्र की आंतरिक अजन्मा आत्मा के साथ एकमय हो जाती है। वह निव्यक्तिकता ही जगत् में जो कुछ भी है उस सबके परम निरहंकार 'अहं' के साथ हमारा एकत्व है।
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।। २५।।
२५. कुछ लोग ध्यान के द्वारा आत्मा के द्वारा अपनी आत्म-सत्ता में आत्मा को देखते हैं; दूसरे लोग उसे सांख्य योग के द्वारा देखते हैं; और दूसरे कुछ व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा देखते हैं।
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ।। २६।।
२६. परन्तु दूसरे लोग स्वयं इसे नहीं जानने के कारण इसके बारे में दूसरों से सुनते हैं और इस प्रकार उसकी उपासना करते हैं; वे लोग भी, जो कुछ उन्होंने सुना है उसके प्रति समर्पण के द्वारा, मृत्यु से परे चले जाते हैं।
यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ।। २७।।
२७. हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन! जो कुछ भी अचर या चर पदार्थ या प्राणी उत्पन्न होता है उसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान।
यह संपूर्ण विस्तृत जगत् केवल पुरुष और प्रकृति है।
यही है वह ग्रंथि जो आपस में नक्षत्रों को बाँधे रखती है:
वे 'दो' जो एक हैं, वे ही समस्त शक्ति का रहस्य हैं,
वे 'दो' जो एक हैं, वे ही वस्तुओं की शक्ति और उनका धर्म हैं।
मौन रहकर, पुरुष की आत्मा प्रकृति और जग का भरण करती है,
उसके कर्म प्रकृति की आज्ञा का लेखा-जोखा हैं।
प्रसन्न, निष्क्रिय, वह उसके पाँवों तले रहता है:
सौंप देता है अपना वक्षस्थल वह प्रकृति के वैश्व नृत्य हित
हमारे जीवन जिस नृत्य की कंपायमान रंगशाला हैं
यदि न होती अंतर में उसकी शक्ति तो कोई सहन न कर पाता,
फिर भी उसके आनंद के कारण उसे कोई नहीं छोड़ेगा।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।। २८ ।।
२८. परमेश्वर सभी जीवों में समान रूप से स्थित है, नाशवानों में वह अविनश्वर रूप से स्थित है; जो ऐसा देखता है वहीं यथार्थ में देखता है।
इस अस्तित्व का स्वामी हमारे अंदर छिपा बैठा है
और अपनी निज शक्ति के साथ लुका-छिपी का खेल खेलता है;
प्रकृति के उपकरण में गुहा 'देव' रमण करता है।
उक्तर्यामी' पुरुष मानव के भीतर अपने निज गृह के समान वास करता है,
उसने जगत् को अपने मनोविनोद का क्षेत्र बना रखा है,
अपनी शक्ति के कार्यों के हित एक बृहत् व्यायामशाला बना रखा है। '
सर्वज्ञाता' होकर वह हमारी अंधकारमयी अवस्था को स्वीकार करता है.
दिव्य होकर पशु अथवा मानव के आकारों को धारण करता है;
'शाश्वत' होकर 'नियति' और 'काल' को स्वीकार करता है,
अमर होकर मृत्युशीलता के साथ मन-बहलाव करता है।
'सर्व-चेतन' होकर 'अज्ञान' में कूदने का जोखिम उठाया,
'सर्व आनंदमय' ने ही संज्ञाहीन होना वहन किया है।
संघर्ष और दुख भरे इस जगत् में अवतीर्ण होकर,
वह हर्ष और शोक का जामा पहन लेता है
और अनुभव को शक्तिदायी वारुणी के समान पान करता है।
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ।। २९॥
२९. जो एक ही ईश्वर को सर्वत्र समान रूप से अवस्थित देखता है, वह अपनी सच्ची आत्मा का अपने निम्न स्व के द्वारा अनिष्ट नहीं करता, और इस प्रकार वह परम गति को प्राप्त हो जाता है।
आध्यात्मिक ज्ञान हमारी अन्तःस्थ आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, इस या उस योग अथवा एकत्व-प्राप्ति के इस या उस मार्ग के प्रति आत्मा की पुकार के द्वारा जागृत हो सकता है। या यह हमें दूसरों से सत्य का श्रवण करने तथा जिसे वह श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनता है उसी सत्य के भाव में मन को ढाल देने से प्राप्त हो सकता है। परंतु चाहे जैसे भी यह प्राप्त हो, यह हमें मृत्यु से परे अमृतत्व की ओर ले जाता है। ज्ञान आत्मा के मृत्युशील प्रकृति के साथ होनेवाले क्षर व्यवहारों से बहुत ऊपर अवस्थित हमारी परमोच्च आत्मा को हमें इस रूप में दिखला देता है कि वे प्रकृति के कर्मों के महेश्वर हैं जो सब पदार्थों और प्राणियों में एक और सम हैं, न किसी देह के ग्रहण के समय जन्म लेते हैं और न ही इन सब देहों के विनाश के समय मृत्यु के अधीन होते हैं। यही यथार्थ देखना है, हमारे अंदर उस सत्ता को देखना जो शाश्वत और अमर है। जैसे-जैसे हम सभी वस्तुओं में इस सम आत्मा को अधिकाधिक अनुभव करते हैं, वैसे-वैसे हम आत्मा की उस समता में प्रवेश करते जाते हैं; जैसे-जैसे हम इन विश्वमय पुरुष में अधिकाधिक निवास करने लगते हैं, वैसे-वैसे हम स्वयं विश्वमय पुरुष बनते जाते हैं; जैसे-जैसे हम इन सनातन के विषय में उत्तरोत्तर सज्ञान होते जाते हैं, वैसे-वैसे हम अपनी सनातनता को धारण करते जाते हैं और सनातन ही बन जाते हैं। हम तब अपने मानसिक तथा भौतिक अज्ञान की सीमा और दुर्दशा के साथ तदाकार न रहकर आत्मा की नित्यता के साथ तदाकार हो जाते हैं।
जैसे-जैसे हमें अधिकाधिक अनुभव होते जाते हैं वैसे-वैसे ही वह चीज हमारे अंदर विकसित होने लगती है।
प्रश्न : 'इस या उस मार्ग' से क्या अर्थ है?
उत्तर : इसका अर्थ है कि महत्त्व इसका नहीं कि किस विशिष्ट मार्ग से व्यक्ति अग्रसर होता है - वह कोई भी मार्ग अपना सकता है - अपितु उस आंतरिक इच्छा का है, उस पुकार का है जो भगवान् के साथ एकत्व-प्राप्ति की चाह रखती है। इसके लिए व्यक्ति कौनसी योग पद्धति अपनाता है, कौनसे विधि-अनुष्ठान अपनाता है इसका कम महत्त्व होता है। यदि भीतर से परमात्मा की प्राप्ति की श्रद्धा न जागृत हुई हो तो सभी कुछ निष्फल है। पर जब एक बार यह श्रद्धा जागृत हो जाए तब फिर सभी पद्धतियाँ इस ओर ले जाने में सहायक हो जाती हैं। और ज्यों-ज्यों व्यक्ति को अंदर से संपर्क प्राप्त होता है, अधिकाधिक अनुभव प्राप्त होते हैं, त्यों ही त्यों वह अधिक तदाकार हो पाता है और इसी कारण वह इस पथ पर टिक पाता है। यदि ऐसा न होता तब तो व्यक्ति उन्हीं क्रिया-कलापों को दोहराता रहता जिनमें सामान्य जन संलग्न रहते हैं और जिनमें कभी इस मार्ग के प्रति कोई चाह नहीं होती। इसलिए मार्ग पर चलने पर अवश्य ही व्यक्ति कुछ हद तक उन सभी सामान्य व्यस्तताओं से ऊपर उठ जाता है। जब भीतर से आत्मा जागृत हो तब कोई भी बाहरी साधन कारगर बन जाता है। उसी के प्रभाव से कोई भी ध्यान, चिंतन, अध्ययन, श्रवण या अन्य कोई भी योग-पद्धति उसे अनुभव तक ले जा सकते हैं। वहीं यदि भीतर से यह पुकार न हो तब ये सभी चीजें केवल बाहरी क्रियाएँ ही रहती हैं जिनका कोई अधिक लाभ नहीं होता। यही नहीं, यदि भीतरी पुकार न हो या फिर वह शुद्ध न हो तो ये सभी अभ्यास अधिकांशतः अहं की तुष्टि के ही साधन बन जाते हैं।
प्रश्न : यहाँ 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग आध्यात्मिक अनुभव को सूचित करता है?
उत्तर : हाँ, अनुभव से ही ज्ञान आता है। परंतु सामान्यतया अनुभव से अर्थ लगाया जाता है कि किसी प्रकार का दर्शन हो जाना, कोई वाणी सुनाई देना, आदि। परंतु अनुभव के विषय में श्रीअरविन्द की परिभाषा सर्वधा भिन्न प्रकार की है। श्रीअरविन्द कहते हैं, "अनुभव एक ऐसा शब्द है जो योग में घटित होने वाली लगभग सभी बातों को समाविष्ट करता है, केवल जब कोई (अनुभव) स्थिर हो जाता है तब वह अनुभव न रहकर सिद्धि का एक अंग बन जाता है; उदाहरणार्थ, जब शांति आती-जाती रहती है तो यह एक अनुभव है - जब वह स्थिर हो जाती है, और फिर नहीं जाती, तब वह एक सिद्धि है। साक्षात्कार भिन्न वस्तु है - जब तुम किसी चीज की अभीप्सा कर रहे हों और वह तुम्हारे सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाए; उदाहरण के लिए तुम्हारे अंदर एक विचार है कि भगवान् सब में विद्यमान हैं, परंतु यह मात्र एक विचार, एक विश्वास ही है; पर जब तुम सबके भीतर भगवान् का अनुभव या दर्शन करने लगो, तब वह साक्षात्कार बन जाता है।" (CWSA 30, p. 5)
"ऐसा कोई नियम नहीं कि कोई भावना अनुभव नहीं हो सकती: अनुभव सभी प्रकार के होते हैं और वे चेतना में हर प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। जब चेतना किसी भी आध्यात्मिक, चैत्य या यहाँ तक कि गुद्ध चीज के अनुभव से गुजरती है, उसे देखती या आभास करती है तो यह (योग के तकनीकी अर्थ में) अनुभव होता है, क्योंकि निःसंदेह बहुत से अनुभव होते हैं जो इस प्रकार के नहीं होते। स्वयं भावनाएँ भी अनेक प्रकार की होती हैं। भावना शब्द प्रायः किसी संवेग के लिए प्रयुक्त होता है, और चैत्य अथवा आध्यात्मिक श्रेणी के संवेग-भावावेग हो सकते हैं जिन्हें यौगिक अनुभवों में गिना जाता है, जैसे कि शुद्ध भक्ति को तरंग अथवा भगवान् के प्रति प्रेम उमड़ना। अंग्रेजी शब्द फीलिंग का अर्थ किसी अनुभूत वस्तु का स्पर्श भी होता है - भले ही यह स्पर्श प्राण में, अथवा चैत्य या चेतना के अपने सारतत्त्व में ही हो। मैंने प्रायः देखा है कि मानसिक स्पर्श भी, जब वह बहुत स्पष्ट हो, फीलिंग कहलाता है। यदि तुम इन्हें तथा इन जैसी अन्य फीलिंग्स को फीलिंग कहकर रद्द कर दो और उन्हें अनुभव न कहो तब तो अनुभवों के लिये बहुत थोड़ा स्थान रह जाएगा। भावप्रधान अनुभूति (feeling) और अंतर्दर्शन आध्यात्मिक अनुभव के मुख्य प्रकार हैं। व्यक्ति ब्रह्म को सर्वत्र देखता और अनुभव करता है; वह एक शक्ति को अपने में प्रवेश करते या अपने से बाहर निकलते देखता है। वह अपने अंदर अथवा चारों ओर भगवान् की उपस्थिति को देखता अथवा महसूस करता है, वह ज्योति के एवं शांति अथवा आनंद के अवरोहण को भी देखता तथा महसूस करता है। यदि तुम इन सबको 'फीलिंग' मात्र कहकर त्याग दो तो जिनको हम अनुभव कहते हैं तुम उनके अधिकतम भाग को रद्द कर दोगे। अब, हम चेतना के तत्त्व, या चेतना की अवस्था में भी एक परिवर्तन महसूस करते हैं, हम शुद्ध विस्तार के एक (सूक्ष्म) क्षेत्र में अपने को फैलता हुआ पाते हैं और शरीर को उस विस्तार में छोटी-सी वस्तु महसूस करते हैं (ऐसा देखा भी जा सकता है), हम अपनी हृत्-चेतना को संकीर्ण होने के बदले विस्तृत, कठोर होने के बदले कोमल, और धूमिल होने के बदले ज्योतिर्मय होते महसूस करते हैं, ऐसे ही मस्तिष्क-चेतना, प्राण और शरीर-चेतना को भी। इसी प्रकार की सहस्रों चीजें हम महसूस करते हैं, भला हम उनको अनुभव क्यों न कहें? निःसंदेह यह एक अंतर्दर्शन, एक आंतरिक भाव, सूक्ष्म-अनुभूतिरूप होते हैं, शीत पवन, पत्थर अथवा अन्य किसी वस्तु की फीलिंग के समान भौतिक नहीं हैं, परंतु ज्यों-ज्यों अंतः-चेतना गहन बनती जाती है ये कम स्पष्ट अथवा कम मूर्त नहीं अपितु अधिक स्पष्ट अथवा मूर्त होते जाते हैं।" (CWSA 30, p. 7)
जब श्रीअरविन्द की परिभाषा के दृष्टिकोण से हम अनुभव को समझने का प्रयास करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अनुभव एक बहुत ही व्यापक शब्द है। यदि आम तौर पर जिसे अनुभव कहते हैं - जैसे कि कोई दर्शन होना, किन्हीं सूक्ष्म सत्ताओं के संपर्क में आना केवल वे ही अनुभव होते तब तो इनका दायरा बहुत ही सीमित हो जाता और साथ ही इन चीजों की कोई विश्वसनीयता भी नहीं थी। यदि व्यक्ति का सभी समय सूक्ष्म जगत् की सत्ताओं के साथ संपर्क रहता है और उनकी सहायता से वह कुछ विलक्षण कार्य भी कर लेता है, या फिर यदि व्यक्ति को सभी समय कोई दर्शन प्राप्त होते रहते हैं तो भी इन सभी चीजों से आवश्यक नहीं कि उसे आत्मा की कोई सच्ची अनुभूति, कोई सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। वहीं, यह भी संभव है कि कोई एक छोटा सा विचार भी गहरा ज्ञान प्रदान कर दे। अतः यह एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है। सामान्यतः जिन्हें हम अनुभव कहते हैं उनके होने या न होने से आंतरिक श्रेष्ठता का कोई मूल्यांकन भी नहीं हो सकता है।
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ।। ३०।।
३०. जो यह देखता है कि सभी कर्म प्रकृति के द्वारा ही किये जाते हैं, और आत्मा कर्ता नहीं है, वह यथार्थ देखता है।
प्रकृति हमारे अन्दर कर्म का गठन करती है; पुरुष इसके अन्दर या इसके पीछे रहकर उसे साक्षीभाव से देखता, अनुमति देता, उसे धारण करता तथा उसका भरण करता है। प्रकृति हमारे मन में विचार (idea) की रचना करती है; इसके अन्दर या पीछे अवस्थित पुरुष उस विचार को तथा उसके अन्तर्निहित सत्य को जानता है। प्रकृति कर्म का परिणाम निश्चित करती है। इसके अन्दर या पीछे अवस्थित पुरुष उस परिणाम को भोगता या सहन करता है। प्रकृति मन और देह की रचना करती है, उन पर परिश्रम करती है। उन्हें विकसित करती है; पुरुष उस रचना एवं विकास को धारण करता है और प्रकृति के कार्यों के प्रत्येक पग को अनुमति देता है। प्रकृति एक संकल्पशक्ति प्रयुक्त करती है जो वस्तुओं में तथा मनुष्यों में कार्य करती है; और पुरुष, जो करना चाहिये उसे अपनी अन्तर्दृष्टि से देख कर, उस संकल्प-शक्ति को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह पुरुष सतही अहं नहीं है, अपितु अहं के पीछे अवस्थित निश्चल-नीरव आत्मा है, शक्ति का स्रोत है, ज्ञान का प्रवर्तक तथा उसका ग्रहीता है। हमारा मानसिक 'मैं' इस आत्मा, इस शक्ति, इस ज्ञान की एक मिथ्या प्रतिच्छायामात्र है। अतः यह पुरुष या यह भरण करनेवाली चेतना, प्रकृति के समस्त कर्मों का मूल, ग्रहीता तथा आधार है, पर यह स्वयं कर्ता नहीं है। सामने की ओर अवस्थित प्रकृति अथवा प्रकृति-शक्ति तथा इसके मूल में विद्यमान शक्ति अथवा चित्-शक्ति या आत्म-शक्ति, - क्योंकि यही दो विश्वजननी की आन्तर तथा बाह्य मुखाकृति हैं, - उस सबका कारण होती है जो कुछ संसार में किया जाता है। विश्वजननी अथवा प्रकृति-शक्ति ही एकमात्र कर्मकर्ती है।
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ।। ३१॥
३१. जब मनुष्य भूतों के पृथक् पृथक् भाव (विविध प्रकार के भूतों) को एक सनातन ब्रह्म में स्थित और उससे ही विस्तृत हुए देखता है, तब वह ब्रह्म को प्रास हो जाता है।
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।। ३२ ।।
३२. हे कौन्तेया अनादि और शाश्वत होने से तथा गुणों से सीमित न होने के कारण यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी कुछ भी कर्म नहीं करता और न ही उससे प्रभावित होता है।
विश्व-क्रिया का यह सब सतही प्रपंच एक ही सनातन के अंदर प्राकृत सत्ताओं का नानाविध भूतभाव है, सब कुछ विश्व-शक्ति के द्वारा उस पुरुष की सत्ता की गहराई के अन्दर अपने 'विचार' के बीजों से ही विस्तारित, अभिव्यक्त तथा अनावृत किया जाता है; परंतु आत्मा यद्यपि हमारी इस देह में उसके क्रिया-व्यापारों को अंगीकार करती है और उपभोग करती है, तो भी उसकी मृत्युशीलता से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह जन्म-मरण से परे शाश्वत है, वह उन व्यक्तित्वों से सीमित नहीं होती जिन्हें वह प्रकृति के अंदर नानाविध रूप से ग्रहण करती है, क्योंकि वह इन सब व्यक्तित्वों की एक ही परम् आत्मा है, त्रिगुण के विकारों से परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं गुणों से अनिर्धारित रहती है, कर्मरत रहते हुए भी कर्म नहीं करती, 'कर्तारम् अपि अकर्तारम्, क्योंकि वह प्रकृति के कर्म को धारण तो करती है पर उसके फलों से आध्यात्मिक तौर पर पूर्णतया मुक्त रहती है, वह समस्त कर्मों का मूल तो है, पर अपनी प्रकृति की क्रीड़ा से किसी प्रकार भी परिवर्तित या प्रभावित नहीं होती।
प्रश्न : इसका क्या अभिप्राय है कि 'प्रकृति हमारे मन में विचार की रचना करती है?
उत्तर : यहाँ विचार से अभिप्राय idea से है न कि thought से, अर्थात् किन्हीं सामान्य क्षुद्र सोच-विचार से नहीं अपितु महत् विचारों से है। महत् विचार जैसे कि 'मूलभूत एकत्व' का विचार, 'अमरता' का विचार, आदि। जब भागवत् सत्य मनुष्य के मन पर प्रभाव डालता है, उस पर अपना प्रतिबिंब डालता है तब अनेकानेक महत् विचारों के रूप में ग्रहण किया जाता है। अधिमानसिक स्तर पर परम विचार विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक विचार में अपने आप को चरितार्थ करने की प्रवृत्ति होती है। परंतु जब वे विचार मानसिक चेतना में अभिव्यक्ति का प्रयास करते हैं तब एक विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि अधिमानस से ऊपा के स्तर पर ही एक व्यापक चेतना में सभी को समाहित और समन्वित किया जा सकता है जबकि निचले स्तर पर ऐसी कोई समन्वयकारी चेतना न होने के कारण सभी विचार एक-दूसरे के ऊपर अपने-आप को लादने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, परमात्मा के विषय में ही कितने भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार हैं। कोई उन्हें परम सत् कहता है, कोई उन्हें निराकार ब्रह्म बताता है, कोई उन्हें सगुण साकार बताता है। चूंकि श्रीअरविन्द ने स्वयं इन सभी के सत्यों को अनुभव किया इसलिए वे कहते हैं कि परमात्मा के विषय में ये सभी अनुभव अपने स्थान पर सही हैं परंतु केवल इन्हीं के अंदर परमात्मा के स्वरूप को सीमित नहीं किया जा सकता। वह तो इन सभी से अनंत रूप से विशाल है। इसलिए जब तक कोई विशाल समन्वयकारी चेतना न हो तब तक विचारों का परस्पर विभ्रम चलता रहता है। ज्यों-ज्यों चेतना का विकास होता जाता है त्यों-त्यों सारे विचार समस्वर होते जाते हैं। पार्थिव विकास में सभी विचारों को अपनी-अपनी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता रहा है ताकि उनके पीछे के सत्य को अभिव्यक्ति मिल सके और साथ ही उनकी सीमितता का भान हो सके। सभी सभ्यताएँ किन्हीं प्रधान विचारों को लेकर चली हैं। उदाहरण के लिए किसी सभ्यता ने सौंदर्य के विचार को प्रधानता दी है, तो किसी दूसरी ने सही विधान या न्यायपूर्ण व्यवहार के विचार को प्रधानता दी है। इस प्रकार अतीत में सभी संस्कृतियों ने अपने-अपने तरीके से भिन्न-भिन्न आदर्शों को अपनाकर उनके अनुसार अपने समाज को निर्देशित करने का प्रयास किया है। और प्रकृति के इन सभी परीक्षणों के परिणामों के विषय में हम जानते हैं। चूंकि ये सभी एकांगी रूप से ही सत्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास रहे हैं इसलिए इन सभी का एक सीमा के बाद अंत निश्चित होता है। श्रीअरविन्द के अनुसार प्रकृति इन सभी परीक्षणों से होते हुए विश्व-राज्य की ओर बढ़ रही है। जब तक विश्व-राज्य स्थापित नहीं होता तब तक हमारी वर्तमान समस्याओं का हल नहीं हो सकता। इस विषय में श्रीअरविन्द कहते हैं। “...यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्यजाति की एकता प्रकृति की अंतिम योजना का अंग है और यह सिद्ध होकर ही रहेगी। परंतु यह होगी उन अवस्थाओं में और सुरक्षा के उन साधनों के साथ जो जाति की जीवन-शक्ति के मूल को अक्षुण्ण तथा उसकी एकता को विविधता से भरपूर रखेंगे।" (CWSA 25. p. 284)
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ।। ३३ ।।
३३. जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश अपने सूक्ष्म होने के कारण प्रभावित नहीं होता उसी प्रकार आत्मा सर्वत्र देहों में स्थित हुआ अलिप्त रहता है।
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ।। ३४ ।।
३४. हे भारत! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है इसी प्रकार क्षेत्र का स्वामी (क्षेत्री) सकल क्षेत्र को प्रकाशित करता है।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ।। ३५।।
३५. जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को तथा प्रकृति से जीवों के मोक्ष को ज्ञान चक्षु के द्वारा देख पाते हैं वे परम् को प्राप्त होते हैं।
जब हम अपनी अंतरस्थ आत्मा की ओर मुड़ते हैं तो वह प्रकृति के संपूर्ण क्षेत्र को रश्मियों की पूर्ण प्रभा से संपन्न अपने निज सत्य से प्रकाशित कर देती है। उस ज्ञान के सूर्य के प्रकाश में हमारे अंदर ज्ञानचक्षु खुल जाता है और तब हम फिर इस अज्ञान में नहीं, अपितु उस सत्य में निवास करने लगते हैं। तब हम देख पाते हैं कि हमारा अपनी वर्तमान मानसिक और भौतिक प्रकृति की सीमा में बँधे रहना एक अंधकारमय भ्रांति थी, तब हम अपरा प्रकृति के नियम, अर्थात् मन और देह के नियम से मुक्त हो जाते हैं, तब हम आत्मा की पराप्रकृति को प्राप्त कर लेते हैं। वह अति भव्य और उच्च परिवर्तन ही, मृत्युशील प्रकृति को उतार फेंकना तथा अमर सत्ता को धारण कर लेना ही अंतिम, दिव्य और अनंत संभूति है।
इस प्रकार तेरहवाँ अध्याय 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग' समास होता है।
चौदहवाँ अध्याय
गुणों से ऊपर
गीता के तेरहवें अध्याय के श्लोकों में कुछ निर्णायक विशेषणों के द्वारा सरसरी तौर पर पुरुष और प्रकृति के बीच जो भेद किये गये हैं, इनकी पृथक-पृथक् शक्ति और क्रियाविधि के जो कुछ संक्षिप्त परंतु अर्थगर्पित लक्षण दिये गये हैं वे, और विशेषकर प्रकृति के गुणों का उपभोग करने के कारण उसकी क्रिया के अधीन देहधारी जीव और गुणों का उपभोग करते हुए भी उनसे परे होने के कारण उनके अधीन नहीं होने वाले परमात्मा के बीच जो भेद किया गया है – ये ही वे आधार हैं जिन पर गीता के मुक्त जीव का, जो अपनी सत्ता के सचेतन धर्म में परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया है, सारा विचार आधारित है। उस मुक्ति एवं एकत्व को, उस दिव्य प्रकृति को धारण करने को, अर्थात् साधर्म्य को वह आध्यात्मिक स्वातंत्र्य का वास्तविक सार तथा अमरत्व का संपूर्ण मर्म बताती है। 'साधर्म्य' को दिया गया परम महत्त्व गीता की शिक्षा की प्रधान बात है।
श्रीभगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।। १॥
१. श्रीभगवान् ने कहाः समस्त ज्ञानों में उच्चतम परम ज्ञान को मैं तुझे फिर कहता हूँ जिसे जानकर समस्त मुनि इस (निम्न) अवस्था से उठकर पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो गये हैं।
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥
२. इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण करके और मेरे सादृश्य को प्राप्त हुए मनुष्य सृष्टि में पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते और विश्व-प्रलय के द्वारा भी व्यथित नहीं होते।
और यह महत् कार्य, मानव-प्रकृति से दिव्य प्रकृति में यह आरोहण, हम एक ईश्वरोन्मुख ज्ञान, संकल्प और उपासना अथवा भक्ति के द्वारा ही कर सकते हैं। क्योंकि, परम देव के द्वारा अपने सनातन अंश के रूप में भेजा हुआ जीव, विश्व-प्रकृति की क्रियाओं में उनका अमर प्रतिनिधि होते हुए भी उन क्रियाओं के स्वरूप के कारण अपनी बाह्य चेतना में अपने-आप को प्रकृति की सीमाकारी अवस्थाओं के साथ तथा एक मन, प्राण और शरीर के साथ तदाकार करने के लिए विवश हो जाता है 'अवशं प्रकृतेर्वशात्' जो अपने आंतर आध्यात्मिक सत्स्वरूप और अपने अंतर्निहित परमेश्वर को भूले हुए हैं। अपने सत्स्वरूप के ज्ञान (आत्मज्ञान) को पुनः प्राप्त करना इस सिद्धि या पूर्णता का अनिवार्य साधन है। आत्म-ज्ञान एवं ईश्वर-ज्ञान के बिना तथा अपनी प्राकृतिक सत्ता के प्रति आध्यात्मिक भाव धारण किये बिना पूर्णता नहीं आ सकती, और इसी कारण प्राचीन प्रज्ञा ने ज्ञान के द्वारा मुक्ति पर इतना अधिक बल दिया, - ज्ञान का तात्पर्य वस्तुओं का बौद्धिक बोध नहीं, वरन् मनोमय प्राणी, मनुष्य, का महत्तर अध्यात्म-चेतना में विकसित होना है। आत्मा की सिद्धि के बिना, अर्थात् आत्मा के दिव्य प्रकृति में विकसित हुए बिना उसकी मुक्ति साधित नहीं हो सकती; तटस्थ ईश्वर अपने मन की मौज या अपने अनुग्रह की किसी मनमानी सनद के द्वारा इसे हमारे लिए साधित नहीं कर देंगे। दिव्य कर्म मुक्ति के लिए कारगर हैं, क्योंकि वे हमें हमारी सत्ता के अंतरस्थ प्रभु के साथ बढ़ते हुए एकत्व के द्वारा इस सिद्धि की ओर तथा आत्मा, प्रकृति और ईश्वर के ज्ञान की ओर ले जाते हैं। दिव्य प्रेम भी कारगर है, क्योंकि उसके द्वारा हम अपनी भक्ति के एकमात्र परम भाजन के साथ उत्तरोत्तर साधर्म्य लाभ करते हैं और उन 'परम' के प्रत्युत्तरशील प्रेम का आवाहन करते हैं ताकि वह हमें उनके ज्ञान की ज्योति से तथा उनको सनातन आत्मा की उत्थान करने वाली शक्ति एवं पवित्रता से परिप्लावित कर दे.... यह वह शाश्वत ज्ञान है, महान् आध्यात्मिक अनुभव है जिसके द्वारा सब मुनियों ने वह परमोच्च पूर्णता प्राप्त की तथा सत्ता के विधान में पुरुषोत्तम' के साथ सारूप्य लाभ किया और अब सदा के लिए उनकी शाश्वतता' में निवास करते हैं, सृष्टि में जन्म नहीं लेते, विश्वप्रलय की व्यथा से उद्विग्न नहीं होते। इस प्रकार यह सिद्धि, यह 'साधर्म्य' अमृतत्व का मार्ग है तथा एक अनिवार्य अबस्था है जिसके बिना जीव सचेतन रूप से सनातन में निवास नहीं कर सकता। यहाँ गीता का जो प्रयास है उसका हमें परिप्रेक्ष्य समझना आवश्यक है। गीता यहाँ यह स्पष्ट कर रही है कि भगवान् ने नवें तथा दसवें अध्याय मैं जो मार्ग बताया है उसके साथ गुणों का क्या संबंध है। वास्तव में तीन गुण क्या हैं इस विषय में तो हम विशद चर्चा पहले कर ही चुके हैं। चौथे अध्याय में भगवान् अवतार के जन्म में और एक सामान्य जीव के जन्म मैं भेद का निरूपण करते हैं। किसी जीव के अंदर वे प्रकृति के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करते हैं जबकि अवतार के रूप में वे अपनी प्रकृति को वशीभूत कर के उसके अध्यक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। जब एक व्यष्टिगत जीव जन्म लेता है तो चूंकि वह अपने स्रोत को भूल जाता है और प्रकृति के वशीभूत होता है इसलिए समष्टि को देखकर भ्रमित हो जाता है। देह, प्राण और मन रूपी सत्ता होने के कारण वह सारे जगत् को तीन गुणों के माध्यम से अर्थात् तमस्, रजस् और सत्त्व के दृष्टिकोण से देखता है। उदाहरण के लिए, तमस् के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने पर व्यक्ति को महसूस होता है कि जिस प्रकार का जगत् है उसमें उसे अपने-आप का भरण-पोषण करना होगा, अपने-आप के लिए जीना होगा। इसमें व्यक्ति पूरी तरह अपने-आप पर और केवल अपने ही सुख-आराम आदि पर केंद्रित रहता है। रजस् के दृष्टिकोण से देखने पर उसे यह महसूस होता है कि अपनी शक्ति के बल पर वह अपना कार्य संसिद्ध कर सकता है। इसलिए राजसिक व्यक्ति को तामसिक की अपेक्षा एक बृहत्तर कार्यक्षेत्र उपलब्ध होता है। सत्त्व प्रधान व्यक्ति चीजों को और बाहरी परिस्थितियों को देखता अवश्य है परंतु वह उनके पीछे के सत्य को जानने की, उनमें सामंजस्य स्थापित करने की चाह रखता है। अतः वह इस संसार की व्याख्या माया के रूप में भी कर सकता है जहाँ चीजों का स्वरूप उनकी प्रतीति से भिन्न है। मन-प्राण और देह रूपी सत्ता होने के कारण मनुष्य में एकांतिक रूप से केवल कोई एक ही गुण हो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक की प्रधानता होते हुए भी अन्य दो गुण भी साथ में रहते हैं। प्रधानतः सात्त्विक होते हुए भी व्यक्ति में तमस् की क्रिया भी हो सकती है और रजस् प्रधान होने पर भी व्यक्ति में सत्त्व की क्रिया हो सकती है। मनुष्य की बुद्धि सात्त्विक होने पर भी प्रायः केवल प्राण और शरीर की ही सेवा में नियुक्त रहती है। विरले ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ बुद्धि प्राण और शरीर पर अपना आधिपत्य रखती हो। अधिकांशतः तो हम प्राण को बुद्धि और शरीर पर निरंकुश शासन करते देखते हैं।
__________________
* ध्यान में रहे कि गीता में कहीं भी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि व्यष्टिभूत आध्यात्मिक सत्ता का अव्यक्त, अनिर्देश्य, या परब्रह्म में, अव्यक्तम् अनिर्देश्यम् में, लय होना ही अमरता का सच्चा अर्थ या उसकी सच्ची स्थिति है या योग का सच्चा लक्ष्य है। इसके विपरीत, आगे चलकर वह अमरता का इस रूप में वर्णन करती है कि वह ईश्वर के अंदर उनके परम धाम में निवास करना है, मयि निवसिष्यसि, परं धाम, और यहाँ उसका वर्णन इस रूप में करती है कि वह अमरता साधम्यं, परां सिद्धिम् है, अर्थात् परम पूर्णता है, अपनी सत्ता और प्रकृति के धर्म में पुरुषोत्तम के समान धर्मवाला होना है, किंतु ऐसा होते हुए भी अस्तित्व में बने रहना तथा विश्व-गतिविधि से सचेतन होते हुए भी उससे ऊपर उठे रहना है, जैसे सब मुनि अभी भी रहते हैं, मुनयः सर्वे, वे सृष्टिचक्र में जन्म के अधीन नहीं होते. युगचक्रों के प्रलय के काल में व्यथित नहीं होते।
* अमर होने का अभिप्राय प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षा में यह कभी नहीं माना गया कि वह केवल देह की मृत्यु के बाद व्यक्ति की सत्ता का बचे रहना ही है: इस अर्थ में तो सभी जीव अमर हैं और केवल उनके बाह्य रूप ही हैं जो नष्ट होते हैं। जो जीव मोक्ष नहीं प्राम कर पाते वे पुनरावर्ती युग-युगांतरों में जीवन-यापन करते हैं, सब भूत व्यक्त लोकों के प्रलय के समय ब्रह्म के अंदर निवर्तित या निगूढ़ रूप में अवस्थित रहते हैं और नए युगचक्र के आविर्भाव के समय पुनः उत्पन्न होते हैं।... गंभीरतर अर्थ में, अमर होने का तात्पर्य मृत्यु के बाद के इस अस्तित्व तथा इस निरंतर पुनरावर्तन से भिन्न है। अमरता वह परा-स्थिति है जिसमें आत्मा को यह ज्ञान होता है कि वह जन्म और मृत्यु से परे है, अपनो अभिव्यक्ति की प्रकृति से परिसीमित नहीं है, अनंत एवं अविनाशी है, अपरिवर्तनीय रूप से शाश्वत है, - अमर है, क्योंकि कभी जन्म न लेने के कारण वह कभी मरती भी नहीं। भगवान् पुरुषोत्तम, जो परमेश्वर और परंब्रह्म हैं, इस अमर सनातनता से नित्य युक्त हैं और कोई देह ग्रहण करने या वैश्व रूपों एवं शक्तियों को सतत् धारण करने से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे सदा इस आत्म-ज्ञान में प्रतिष्ठित रहते हैं। उनकी प्रकृतिमात्र ही है अपनो निज शाश्वतता के प्रति अपरिवर्तनीय ढंग से सचेतन रहना; वे अनादि और अनंत रूप से आत्म-चेतन हैं। वे यहाँ सभी देहों के अंतर्वासी हैं, परंतु प्रत्येक शरीर में वे अजन्मा के रूप में विद्यमान हैं, उस अभिव्यक्ति के द्वारा वे अपनी चेतना में सीमित नहीं होते, जिस भौतिक प्रकृति को वे धारण करते हैं उससे तदाकार नहीं हो जाते: क्योंकि वह तो उनकी सत्ता के लीलामय जगद्-व्यापार की एक गौण घटना मात्र है।
इसीलिए श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि, "परम देव के द्वारा अपने सनातन अंश के रूप में भेजा हुआ जीव, विश्व-प्रकृति की क्रियाओं में उनका अमर प्रतिनिधि होते हुए भी उन क्रियाओं के स्वरूप के कारण अपनी बाह्य चेतना में अपने-आप को प्रकृति की सीमाकारी अवस्थाओं के साथ तथा एक मन, प्राण और शरीर के साथ तदाकार करने के लिए विवश हो जाता है 'अवशं प्रकृतेर्वशात्' जो अपने आंतर आध्यात्मिक सत्स्वरूप और अपने अंतर्निहित परमेश्वर को भूले हुए हैं।" अतः, जोव जब अपने आप को किसी एक मन, प्राण और शरीर से तदाकार कर लेता है और साथ ही विश्व-प्रकृति की क्रियाओं से विमोहित हो जाता है तब यही सारी समस्याओं का, चेतना के अंधकार का कारण बन जाता है। तो प्रश्न उठता है कि व्यक्ति इस अंधकार से बाहर कैसे निकले? इसके उत्तरस्वरूप भगवान् कहते हैं कि इसके लिए ज्ञान का आश्रय लेना चाहिये। ज्ञान का अर्थ है कि व्यक्ति अपने बोध के लिए अपनी इंद्रियों और बाहरी साधनों पर आश्रित न रहकर आंतरिक रूप से बोध प्राप्त करे। इसे जागृत करने में भगवान् के प्रति प्रेम भी बहुत ही कारगर है। यदि भगवान् के प्रति प्रेम हो, उनके प्रति पुकार हो तो उसका प्रत्युत्तर हमारे अंदर स्वयं ही सभी आवश्यक सद्गुण ले आता है। यदि प्रेम हो तो ज्ञान, सिद्धि आदि तो सहज ही उसके साथ ही साथ चले आते हैं। इसलिए प्रेम भी इस अंधकार से बाहर निकालने में प्रभावी है। साथ ही इससे बाहर निकालने में दिव्य कर्म भी प्रभावी हैं। जब वास्तव में ही व्यक्ति कर्मयोग करता है तो उसके सारे भाग भगवान् की प्रकृति के यंत्र बन जाते हैं और जब भगवान् की दिव्य प्रकृति उनके द्वारा अभिव्यक्त होने लगती है तब धीरे-धीरे वह उस अंधकार को नष्ट कर देती है। अतः जब किसी भी तरीके से व्यक्ति इस अंधकार से निकल जाएगा तो वह साधर्म्य, सारूप्य या सालोक्य प्राप्त कर सकता है।
एक सच्चे दृष्टिकोण से तो गुणों का अपने-आप में कोई अस्तित्व ही नहीं है। एकमात्र भगवान् की पराप्रकृति की ही क्रिया हो रही है जो कि सभी गुणों से परे है। परंतु उसकी क्रिया हमारी मानसिक, प्राणिक और भौतिक चेतना को त्रिगुणमयी प्रतीत होती है। और चूंकि उसको क्रिया हमें गुणमयी प्रतीत होती है तो हम उससे विमोहित हो जाते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि सारा ही व्यापार भगवान् और उनको पराप्रकृति के बीच की क्रीड़ा है। परंतु चूँकि हम इसमें बद्ध हैं इसलिए हमें कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग का सहारा लेना होता है ताकि हम इस निम्न क्रिया से बाहर आ सकें।
प्रश्न : पहली पादटिप्पणी में कहा गया है कि मुनि सृष्टिचक्र के अधीन नहीं होते, तो क्या वे इससे मुक्त होते हैं?
उत्तर : श्रीमाताजी व श्रीअरविन्द के कथनानुसार कुछ चुने हुए ऋषिगण ईश्वरकोटि होते हैं न कि जीव कोटि। वे इस पार्थिव विकासक्रम से नहीं आए हैं अपितु निवर्तन (involution) की प्रक्रिया से आए हैं और इसलिए वे स्वतःसिद्ध और पूर्ण हैं। उन पर इस विकासक्रम को विषमताओं का प्रभाव नहीं होता। पार्थिव जन्म ग्रहण करने पर भी वे पार्थिव क्रियाओं के अधीन नहीं होते। वे अपने निहित उद्देश्य को पूर्ति के लिए आविर्भूत होते हैं और उद्देश्य पूर्ति के बाद पुनः लौट जाते हैं। और जब भी आवश्यकता होती है तब वे पुनः लौटकर इस पार्थिव अभिव्यक्ति में आ जाते हैं। श्रीमाताजी व श्रीअरविन्द के अनुसार ऋषियों का एक समूह सदा ही पार्थिव विकास में सहायता प्रदान करता आया है। वे ही ऋषि अलग-अलग समयों में अलग-अलग शरीर धारण कर इस विकासक्रम को आगे गति प्रदान करते हैं। उन्हीं आत्माओं के लिए गीता कहती है 'सर्वभूत हिते रताः', वे सदा ही सभी जीवों के कल्याण में रत रहते हैं।
प्रश्न : क्या सामान्य जीव ईश्वरकोटि भाव में जा सकता है?
उत्तर : किसी जीव के लिए ईश्वरकोटि बनना संभव नहीं है। हमारे इस पार्थिव जगत् का स्वरूप क्रमविकासमय है जिसमें व्यक्ति सदा ही उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है और चेतना के अधिकाधिक उच्च स्तरों पर आरोहण करता जाता है। परंतु चूंकि परम् सत्ता अनन्त है इसलिए इस आरोहण का भी कोई अंत नहीं है। ऐसे में अत्यंत उच्च स्तरों पर आरोहण कर चुके होने के बाद भी व्यक्ति के आगे आरोहण के अनंत सोपान शेष रहते हैं और इस प्रकार यह आरोहण चलता रहता है। परंतु इसमें जीव ईश्वरकोटि नहीं बन जाता। ईश्वरकोटि भाव तो केवल अवतरण से ही आ सकता है। इसमें यह अवश्य ही संभव है कि स्वयं वह भाव किसी जीव में अवतरित हो जाए जिस कारण वह जीव ईश्वरकोटि बन जाए। परंतु फिर भी इस भाव में जाने की प्रक्रिया अवतरण से ही हो सकती है किसी प्रकार के क्रमविकास से नहीं।
प्रश्नः दूसरी पादटिप्पणी में कहा गया है कि, "अमरता वह परा-स्थिति है जिसमें आत्मा को यह ज्ञान होता है कि वह जन्म और मृत्यु से परे है", तो क्या अन्य स्थितियों में व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता?
उत्तर : यहाँ किसी कोरे मानसिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। इस ज्ञान का अर्थ है जीवंत रूप से आत्मा का उस चेतना में निवास करना जहाँ वह जन्म और मृत्यु दोनों को समान ही रूप से अपनी अभिव्यक्ति के काम में लेती है।
प्रश्न : जब हम मोक्ष की बात करते हैं क्या वह मानसिक चेतना से ऊपर की बात नहीं है?
उत्तर : हमें यह ध्यान में रखना होगा कि अभी तक मनुष्य मानसिक चेतना से ऊपर नहीं गए हैं। इसलिए उससे परे की चीज का तो उसे कोई आभास ही नहीं हो सकता। कोई भी बड़े-से-बड़ा ऋषि भी अभी तक भानासिक चेतना के परे नहीं जा सका है। आज तक जो भी ऊँचे से ऊँचे अनुभव प्राप्त हुए हैं वे सब मन के माध्यम से ही हुए हैं न कि स्वयं उस स्तर पर जाकर। इस पार्थिव अभिव्यक्ति में मनुष्य अब तक मानसिक चेतना से आगे नहीं जा पाया है। जब हम उच्चतर लोकों में आरोहण की बातें करते हैं तो मानव सत्ता का केवल एक भाग ही है जो यह आरोहण करता है। शेष सारी सत्ता आरोहण नहीं कर पाती और निचले स्तर पर ही बनी रहती है। और जो भाग आरोहण करता है यदि वह प्रभावी होता है तो साधक को अवश्य ही उस भाग में अमरता का भान हो सकता है। सामान्यतया हमारे आध्यात्मिक साहित्यों में हम जिन साक्षात्कार और अनुभूति आदि का वर्णन पढ़ते-सुनते हैं वह तो चेतना की अनंत स्तर परंपरा में एक बहुत ही निचले स्तर की बात है और वे भी मन, प्राण और शरीर के माध्यम से ही होते हैं। यहाँ तक कि सच्चिदानंद का अनुभव भी आज तक केवल हमारी निम्न सत्ता एवं मानसिक सत्ता के माध्यम से ही हुआ है। जब हम मानसिक चेतना या सत्ता की बात करते हैं तो उसमें मानव मन से ऊपर उच्चतर मन (Higher Mind), ज्योतिर्मय मन (Illumined Mind), अंतर्भासात्मक मन (Intuition) और अधिमन (Overmind) भी शामिल हैं। उसके अपने स्तर पर सच्चिदानंद के साक्षात्कार की तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। श्रीअरविन्द ने चेतना के विभिन्न स्तरों की योजना का जो नक्शा बताया है उसमें तो अतिमानसिक स्तर भी बहुत ही निचले स्तर पर है जबकि हमारे लिए तो यह हमारी किन्हीं भी कल्पनाओं से भी सर्वथा परे की बात है।
मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ।
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।। ३।।
३. हे भारत! महत्-ब्रह्म मेरा गर्भाशय है, उसमें मैं बीज का आधान करता हूँ, उससे समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।। ४।।
४. हे कौन्तेय! समस्त जीव योनियों में जो देहादिरूप आकृतियाँ उत्पान होती हैं उन सबका गर्भाशय महत्-ब्रह्म है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ।
यदि मनुष्य की अंतरात्मा अपने गुप्त सारतत्त्व में भगवान् के साथ अविनाशी रूप से एक न होती तथा उनकी दिव्यता का ही अंश न होती तो वह उनके साथ साधर्म्य लाभ न कर सकती थी... निश्चय ही हम निम्नतर जड़ प्रकृति में आये हुए हैं और उसके प्रभाव के अधीन हैं, पर हम यहाँ आये हैं उस परम आध्यात्मिक प्रकृति से ही : यह अधीनस्थ अपूर्ण स्थिति हमारी बाह्य गोचर सत्ता है, परंतु वह (उच्चतर) ही हमारी सच्ची सत्ता है। सनातन इस समस्त जगत्-क्रिया को अपनी आत्म-सृष्टि के रूप में उत्पन्न करते हैं। वे एक ही साथ इस विश्व के पिता और माता हैं; अनंत विज्ञान-तत्त्व, महत् ब्रह्म, ही वह योनि है जिसमें वे अपने आत्म-आधान का बीज डालते हैं। अधि-आत्मा (Over-Soul) के रूप में वे बीज डालते हैं; जगज्जननी, प्रकृति-आत्मा, अपनी सचेतन शक्ति से परिपूर्ण चित्-शक्ति के रूप में वे इसे सत्ता के इस अनंत तत्त्व में ग्रहण करते हैं जो उनके असीम पर आत्म-परिसीमक विज्ञान से गर्भित कर दिया जाता है। इस महत् आत्म-आधान में वे उस दिव्य बीज को ग्रहण करते हैं और वहाँ गर्भाधानमय सृजन की मूल क्रिया के द्वारा दिव्य भ्रूण को सत्ता के मानसिक तथा भौतिक आकार में विकसित करते हैं। जो कुछ भी हम यहाँ देखते हैं वह सब उसी सृजन-क्रिया से उद्भूत होता है; परंतु जो कुछ यहाँ उत्पन्न होता है वह उन अजन्मा तथा अनंत का केवल एक सीमित भाव और रूप है।
हालाँकि गीता में तो इस विषय को अधिक विस्तार से नहीं समझाया गया है परंतु अपनी वेद-विषयक कृतियों में श्रीअरविन्द ने इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।
मोटे रूप से हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि सारी सृष्टि भगवान् की पराप्रकृति द्वारा होती है। परमात्मा जहाँ कहीं भी अपना दृष्टिपात करते हैं वहीं मानो वे अपनी पराप्रकृति को अभिव्यक्ति के उन तत्त्वों से, उन पहलुओं से निषेचित कर देते हैं और पराप्रकृति उन सभी तत्त्वों को अभिव्यक्त करती हैं। जब ये पहलू अतिमानसिक चेतना में अभिव्यक्त होते हैं तब उस स्तर पर ये सभी एकमय और समन्वित होते हैं। परंतु ज्यों-ज्यों ये पहलू या तत्व नीचे मानव मन के स्तर पर आते हैं त्यों-त्यों उन सब में जो एकात्मकता और समस्वरता होती है वह अपना वैसा स्वरूप नहीं रख पाती और वे भिन्न-भिन्न महत् विचारों का रूप ले लेते हैं। परंतु मानसिक स्तर पर हम उन सब तत्त्वों के भीतर के समन्वयकारी तत्त्व को नहीं देख पाते इसी लिए प्रायः ही ये महत् विचार एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े प्रतीत होते हैं जबकि अपने उद्गम में ये सारे एक ही सत्ता के पहलू होते हैं। इसलिए मानसिक विकास और संस्कार की प्रक्रिया में हम किसी विचार को स्थापना (thesis) और उसकी प्रतिस्थापना (anti- thesis) पर विचार करते हैं और फिर उन्हें समन्वित करने का प्रयास करते हैं। इससे मन का विकास होता है और उसमें रूढ़िवादिता से कुछ मुक्ति मिलती है तथा उसमें कुछ अधिक नमनीयता आती है जिससे कि हम सत्य के कुछ अधिक नजदीक पहुँचते हैं।
और अपने मूल में जो महत् विचार थे वे ही अभिव्यक्ति में आकर छोटे विचारों का रूप ले लेते हैं जो कि और निचले स्तर पर प्राणिक आवेगों आदि का और उससे नीचे भौतिक वृत्तियों का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार यह निवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें अपने अतिचेतन मूल से चलकर चीजें हमारे जड़भौतिक स्तर तक और उससे भी नीचे के स्तरों तक पहुँचती है। हालाँकि हम इस निवर्तन की प्रक्रिया के विषय में सचेतन नहीं होते। हम तो केवल क्रमविकासमय जगत् के विषय में हो सचेतन होते हैं।
हमारी वैदिक परंपरा में शब्द और ध्वनि को ही सारी सृष्टि का मूल बताया गया है। उनके अनुसार मंत्र से ही सारी सृष्टि होती है। मंत्रों की ध्वनियों में वह शक्ति निहित होती है जो विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्त्र परिणाम उत्पन्न कर सकती है।
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ।। ५॥
५. हे महाबाहो! प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण अविनाशी देहधारी जीवात्मा को देह में बाँधते हैं।
वह कौन-सी चीज है जो जीव को जन्म, मृत्यु और बंधन को बाह्य प्रतीति कराती है, - क्योंकि यह तो सर्व-विदित है कि यह एक प्रतीति मात्र ही है? यह चेतना की एक गौण क्रिया या अवस्था है, यह इस प्रकार को निम्नतर प्रेरणा की सीमाबद्ध क्रियाओं में प्रकृति के गुणों के साथ तथा मन-प्राण-शरीर की इस आत्म-परायण अथवा स्व-केंद्रित अहंबद्ध कर्म को ग्रंथि के साथ हमारी आत्म-विस्मृतिपूर्ण तदात्मता है। यदि हमें निम्नतर किना की विमोहक शक्ति से परे हटकर अपनी पूर्ण-सचेतन सत्ता में पुनः प्रका करना है और आत्मा की मुक्त प्रकृति तथा उसकी नित्य अमरता को धारणा करना है तो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना, त्रैगुण्यातीत होना परमावश्यक है। यही वह साधर्म्य की अवस्था है जिसकी व्याख्या करने की ओर गीता इसके बाद अग्रसर होती है। पहले एक अध्याय में वह इसकी ओर संकेत कर ही चुकी है और कुछ बल के साथ इसका प्रतिपादन भी कर चुकी है; परन्तु अब उसे अधिक सुनिश्चित शब्दों में यह बतलाना है कि ये गुण क्या हैं, जीव को ये किस प्रकार बाँधते तथा आध्यात्मिक स्वातंत्र्य से दूर रखते हैं, तथा प्रकृति के गुणों से ऊपर उठने का क्या अभिप्राय है?
प्रश्न : श्रीअरविन्द यहाँ टीका में कहते हैं कि जीव को जन्म, मृत्यु और बंधन की केवल प्रतीति होती है, वास्तव में कोई बंधन है नहीं, तो इसका वास्तव में अभिप्राय क्या है?
उत्तर : जो ज्ञानी है वह जान चुका होता है कि यह एक प्रतीति मात्र है। परंतु जो अज्ञान में है उसे तो यह यथार्थ ही प्रतीत होता है। इसलिए यह प्रतीति मात्र है या यथार्थ यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इससे कितना तादात्म्य रखता है। यदि वह पूरी तरह इससे तदात्म है, इसमें फँसा हुआ है, तो उसे सारी चीजें यथार्थ प्रतीत होंगी और चूँकि वे उसके लिए यथार्थ होंगी इसलिए वह उनसे हर्ष-शोक, सुख-दुःख आदि भी अनुभव करेगा।
जैसा कि हम अनेक बार इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि मूलतः तो गुणों का आभास भी केवल प्रतीति मात्र ही है क्योंकि परम प्रभु और उनकी चित् शक्ति परा प्रकृति के अतिरिक्त तो संसार में और कुछ है ही नहीं। सब कुछ उन्हीं की क्रीड़ा है जो वे अपने आनन्द के लिए करते हैं। और ये दो भी भिन्न नहीं अपितु एक ही हैं। हम मनुष्य और उसकी चेतना का रूपक देकर परम प्रभु और उनकी चित् शक्ति की अभिन्नता बताने का प्रयास करते हैं परंतु वास्तव में वे उससे भी कहीं अधिक अंतरंग रूप से एक हैं। और परम प्रभु के स्वरूप को हम ज्ञान, सत्य, प्रेम, सौंदर्य आदि जिन भी मानवीय परिभाषाओं से अलंकृत करने का प्रयास करते हैं वे भी उनकी लीला के मोहरे मात्र हैं, उनका सत्स्वरूप तो हमारी किन्हीं भी मानसिक परिभाषाओं से अनंततः परे है। हमारी मानवीय चेतना के लिए बहुत सी चीजें तो असहनीय होती हैं और हम समझ नहीं पाते कि भगवान् ऐसी वीभत्स चीजों में आनंद कैसे लेते होंगे परंतु वास्तव में तो वे हमारी मानवीय नैतिकता के लिए ही घृणास्पद होती हैं। हमारे कोई भी नैतिक विधान भगवान् पर लागू नहीं होते। जिस प्रकार मानव चेतना पशुओं के विधान के अनुसार नहीं चल सकती उसी प्रकार मनुष्यों के चातिक विधान परमात्मा पर बाध्यकारी नहीं होते। इसीलिए जब हम अपनी नैतिकता आदि के मानदंडों पर परमात्मा की क्रियाओं का आकलन करने का प्रयास करते हैं तब यह एक भारी त्रुटि होती है। इसी कारण जब आज का शिक्षित मन वृंदावन की लीला और रास के विषय में पढ़ता है तब उसे यह एक घोर विलासिता और अनैतिकता भरा कल प्रतीत होता है क्योंकि हम इस रूपक से यह नहीं समझ पाते कि यह तो अपने आनन्द के लिए परंब्रह्म, परमात्मा की लीला है और चूंकि हम कामना-वासना के अतिरिक्त कुछ सोच नहीं सकते इसलिए भगवान् की लीला के ऊपर भी हम अपनी दूषित मानसिकता अध्यारोपित कर देते हैं, जबकि रास में किन्हीं गुणों का तो कोई प्रवेश ही नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषियों को इस रहस्य का गहरा बोध था और वे जानते थे कि संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा और जगदंबा का क्रीड़ाक्षेत्र ही है। वे ही अपने आप को मुक्त रूप से अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस अभिव्यक्ति में भले हमारी मानसिकता को गुण आदि की प्रतीति हो, परंतु अपने-आप में कोई गुण हैं ही नहीं।
जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो इसके विषय में भी भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं। श्रीअरविन्द के अनुसार अतिचेतन स्तरों से जब अवरोहण और निवर्तन (involution) की प्रक्रिया चलती है तब अवरोही क्रम में अनेकानेक स्तरों में चेतना घनीभूत होती जाती है जिन्हें वे सच्चा मन, सच्चा प्राण आदि कहते हैं और इस प्रकार घनीभूत होते हुए यह प्रक्रिया निश्चेतन स्तरों तक पहुँच जाती है। इन सच्चे लोकों या स्तरों में वे विकृतियाँ नहीं होतीं जो कि क्रमविकासमय स्तरों में होती हैं। जब चेतना निश्चेतन स्तर पर पहुँच जाती है तब यह चेतना का एक पूर्ण विपर्यय हो जाता है जिससे पुनः आरोहण संभव बनाने के लिए भगवान् स्वयं निश्चेतन में स्थित हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत् (१०.८९.५८) में भी हम भूमा पुरुष का उल्लेख पाते हैं जो कि हजार फणों वाले अनंत पर विराजमान महाविष्णु हैं। वे ही इस आरोहण को अग्रसर करने के लिए अवतरित होते हैं और इस क्रमविकास को आगे बढ़ाते हैं अन्यथा निश्चेतना के दबाव के कारण किसी प्रकार का कोई क्रमविकास संभव ही नहीं होता। जिसे हम जड़भौतिक तत्त्व कहते हैं वह तो उस निश्चेतना से एक सुदीर्घ विकासक्रम के बाद ही आ पाया है। वह निश्चेतना तो किसी भी चेतना का इतना पूर्ण रूप से विपर्यय है कि उसमें किसी प्रकार की रिक्तता की भी संभावना नहीं है। जड़भौतिक के एक सुदीर्घ विकास के बाद जीवन का प्रादुर्भाव हुआ। जड़भौतिक तत्त्व में प्राण के संचार के बाद चीजों के प्रति उसमें कुछ-कुछ अहसास पैदा होता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राण भी बहुत अविकसित होता है और चीजों के बोध करने का उसका अपना संकीर्ण तरीका होता है। प्राण के कुछ-कुछ विकास के बाद उसमें अधिक जटिल भावों का अहसास होता है और प्राण के विकास के साथ ही साथ जब मानसिकता का विकास होता है तो उसके अपने तरीके के बोध होते हैं। चूंकि ऐसी विषम पार्थिव परिस्थितियों में जीवन को बनाए रखना पहली आवश्यकता होती है तभी कालांतर में किसी प्रकार की कोई भागवत् अभिव्यक्ति संभव हो सकती है, इसलिए अधिकांशतः मन भी प्राण की ही सेवा में रत रहता है। मनुष्य के प्रादुर्भाव से पहले भी कुछ स्तनधारी जीवों में हम कुछ-कुछ प्राथमिक मानसिकता के चिह्न देख सकते हैं। उसके बाद प्रकृति मानव का निर्माण करती है जो कि सही रूप में मानसिकता को धारण कर सकता है, हालाँकि वर्तमान में तो अधिकांश मनुष्य भी एकांतिक रूप से अपनी निम्न प्राणिक और भौतिक लालसाओं आदि की ही पूर्ति करने में रत दिखाई देते हैं। इसलिए अधिकांश का केवल शरीर ही मनुष्य का है परंतु वास्तव में उनकी सारी क्रियाएँ पशुवत् ही हैं। मूलतः मानसिक चेतना प्राणिक का आधार है और प्राणिक भौतिक का परंतु चूँकि क्रमविकास में आरोहण का क्रम अवरोहण से उल्टा आता है इसलिए जड़भौतिक तत्त्व पहले आता है और प्राण उसके बाद और मानसिकता उसके बाद। क्रमविकास में ये भाग एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्राणिक स्तर भौतिक से अनंनतः विशाल होने पर भी हम देखते हैं कि पार्थिव अभिव्यक्ति में देह नष्ट होने पर प्राण का आधार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही देह और प्राण मानसिकता में प्रवेश करते हैं और उसे प्रभावित करते हैं।
हमारे ये तीनों भाग अपने-अपने तरीके से चीजों की अनुभूति करते हैं, अपने-अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। भौतिक वृत्तियों को हम तामसिक कहते हैं। जिस हद तक भौतिकता हमारे प्राण और हमारे मन में प्रवेश कर के उनके बोध को प्रभावित करती है उस हद तक उनके बोध भी तामसिक होते हैं। उसी प्रकार प्राणिक वृत्तियों को राजसिक कहते हैं। ये पाणिक वृत्तियाँ भौतिक और मानसिक भागों में घुली-मिली होती हैं और उन्हें प्रभावित करती हैं इसलिए उन भागों में भी कुछ-कुछ राजसिकता का प्रवेश हो जाता है। इसी प्रकार मानसिक सत्ता के दृष्टिकोण, चीजों को देखने के उसके तरीके को सात्त्विक कहते हैं। मन चीजों के पीछे के सत्य को, उनके बीच सामंजस्य को, किसी नैतिक विधान आदि को खोजता है इसलिए उसे सात्त्विक कहा गया है। हमारे तीनों ही भाग एक दूसरे में घुले-मिले हुए होते हैं और जिस हद तक जिस भाग का प्राधान्य रहता है उसी के अनुसार व्यक्ति प्रधान रूप से तामसिक, राजसिक और सात्त्विक कहा जाता है। वास्तव में तो तामसिक, राजसिक और सात्त्विक की प्रतीति भी हमें अपनी बद्ध चेतना के कारण ही होती है, अन्यथा यथार्थतः तो सारा जगत् भगवान् शिव और पार्वती की क्रीड़ा ही तो है और यह सारी अभिव्यक्ति उन्हीं के आनन्द के लिए है। परंतु चूंकि हमारी चेतना इसमें बद्ध है और हमें यही यथार्थ प्रतीत होता है इसीलिए हमें सुख-दुःख, राग-द्वेष आदि भावों से गुजरना होता है। भले किसी दृष्टिकोण से यह सारा संसार प्रतीति मात्र ही है और इसमें कोई यथार्थता नहीं है परंतु हमारी चेतना के लिए यथार्थ होने के कारण हमें तो इसमें माँतक दुःख-कष्ट और यंत्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं। परंतु कुछ सूक्ष्म विश्लेषण में हम पाते हैं कि यह सब केवल प्रतीति मात्र ही है। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करता है कि जड़भौतिक जैसी कोई चीज नहीं है, सब कुछ सूक्ष्म ऊर्जा के कारण ऐसा प्रतीत होता है। अतः भारतीय परंपरा में सदा ही इस चीज का भान रहा है कि यह सारी प्रतीति आत्मपरक है। किसी एक को यह जगत् जिस प्रकार का गोचर होता है वैसा किसी दूसरे को गोचर नहीं होता। और पशु चेतना को जिस प्रकार का यह जगत् गोचर होता है वैसा मानव चेतना को गोचर नहीं होता। कुछ ऐसी सत्ताएँ हैं जिनका गठन सर्वथा भिन्न प्रकार का होता है। उनके लिए हमारे जड़भौतिक जगत् का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए वास्तव में तो किन्हीं भी दो जीवों को यह जगत् एक जैसा गोचर नहीं होता। यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति को भिन्न-भिन्न समयों पर यह भिन्न-भिन्न गोचर होता है। केवल कुछ चीजों में समानता प्रतीत होती है अन्यथा सभी कुछ भिन्न होता है। और यह समानता का भाव भी इसलिए होता है ताकि एक व्यवस्था बनी रहे।
प्रश्न : यहाँ आत्म-विस्मृति से क्या अर्थ है?
उत्तर : आत्म-विस्मृति का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के संपर्क में नहीं होता। और ज्यों ही व्यक्ति अपनी आत्मा के संपर्क में आता है त्यों ही वह अपनी वास्तविकता जान जाता है और अपने मन, प्राण, शरीर रूपी बाहरी उपकरणों तथा उनकी वृत्तियों को समझ जाता है और तब वह अधिक सच्चे रूप से चीजों को देखने लगता है। और जब व्यक्ति अपने मन, प्राण और शरीर से तादात्म्य रखता है तब वह इनके चंगुल में फंसकर इनके द्वारा ही अपने सारे क्रिया-कलाप करने लगता है और ऐसे में उसकी आत्मा को अपनी वाणी सुनाने का अवसर कम या बिल्कुल नहीं मिलता। हमारी वर्तमान संस्कृति में जब व्यक्ति बाहरी चीजों से स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है तो यह उसकी आत्म-विस्मृति का अचूक चिह्न है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि पग-पग पर अपने मार्गदर्शन के द्वारा लोगों को सच्ची दिशा दिखाकर उन्हें एकांगी रूप से अपनी निम्न वृत्तियों की तुष्टि करने से सदा ही रोकते थे। समाज के सामने सदा ही यह आदर्श रखा जाता था कि जीवन का सच्चा उद्देश्य तो केवल परमात्मा से एक होना ही हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिस किसी भी वर्तमान स्थिति से उस उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकता है, और ऐसा किया जाना इसलिए सुगम है क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं वे परमात्मा ही हैं। आध्यात्मिक आदर्श के प्रभाव के कारण ही हम पाते हैं कि भारतीय समाज उन विभीषिकाओं से सुरक्षित रहा जो हमें घोर सुखभोगवादी संस्कृतियों में दिखाई देती हैं जिनमें सदा ही व्यक्ति पर किसी भागवत् प्रभाव के अभाव में निम्न वृत्तियों का अधिकार हो जाता है और उसकी आत्मा कुंठित हो जाती है। आध्यात्मिक आदर्श की इसी अपरिहार्यता को अनुभव करते हुए स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि, "प्रत्येक व्यक्ति की भाँति प्रत्येक राष्ट्र का भी एक विशेष जीवनोद्देश्य होता है, एक विशिष्ट जीवनधारा होती है जो कि उसके जीवन का केन्द्र, उसके जीवन का प्रधान स्वर होता है, जिसके इर्द-गिर्द अन्य सब स्वर मिलकर समरसता उत्पन्न करते हैं। किसी एक देश में, जैसे इंग्लैंड में, राजनीतिक शक्ति या सत्ता ही उसकी जीवन-शक्ति होती है और इसी प्रकार किसी अन्य देश में उसकी जीवन-शक्ति होतो है कलाकौशल की उन्नति करना, और ऐसे ही भिन्न राष्ट्रों का भिन्न-भिन्न प्रधान लक्ष्य, उनकी भिन्न-भिन्न धारा होती है। किन्तु भारतवर्ष में धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केन्द्र है और वही राष्ट्रीय जीवनरूपी संगीत का प्रधान स्वर है। यदि कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक जीवनी-शक्ति को दूर फेंक देने की चेष्टा करे - शताब्दियों से जिस दिशा की ओर उसको विशेष गति रही है, उससे मुड़ जाने का प्रयत्न करे - और यदि वह अपने इस प्रयास में सफल हो जाए, तो वह राष्ट्र मर जाता है। अतएव यदि तुम धर्म को फेंककर राजनीति, समाज-नीति अथवा अन्य किसी दूसरी नीति को अपना केन्द्र, अपने राष्ट्रीय जीवन की जीवनी-शक्ति बना लो, तो उसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारा अस्तित्व तक न रह जाएगा। यदि तुम इससे बचना चाहो या चाहो कि ऐसा न हो, तो अपने धर्म की जीवनी-शक्ति के द्वारा ही अपने सारे कार्य करने होंगे, अपनी प्रत्येक क्रिया का केन्द्र इस धर्म को ही बनाना होगा। तुम्हारे स्नायुओं का प्रत्येक स्पन्दन तुम्हारे इस धर्मरूपी मेरुदंड के द्वारा स्पंदित हो। मैंने देखा है कि सामाजिक जीवन पर धर्म का व्यावहारिक प्रभाव कैसा पड़ेगा यह उन्हें बिना दिखाये मैं अमेरिकावासियों को धर्म का भी उपदेश नहीं कर सकता था। बिना यह दिखाए कि वेदान्त कौन से आश्चर्यजनक राजनीतिक परिवर्तन ला सकेगा, मैं इंग्लैंड में भी धर्म का प्रचार नहीं कर सका। इसी भाँति, भारत में सामाजिक सुधार का प्रचार केवल यह दिखा कर ही हो सकता है कि यह नवीन प्रणाली कितना अधिक आध्यात्मिक जीवन ला पाएगी; और राजनीति का प्रचार भी यह दिखाकर करना होगा कि वह उस एकमात्र वस्तु – उसकी आध्यात्मिकता- को कितना उन्नत कर सकेगी जिसकी कि राष्ट्र को सर्वाधिक आकांक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना चयन स्वयं करना होता है, उसी भाँति प्रत्येक राष्ट्र को भी। हमने युगों पूर्व अपना पथ चयन कर लिया था, और अब हमें उस पर दृढ़ बने रहना होगा। और आखिर, हमारा चयन उतना कोई बुरा भी नहीं है। जड़ के बदले चैतन्य का, मनुष्य के बदले ईश्वर का चिन्तन करना क्या संसार में इतनी बुगे बात है? परलोक में दृढ़ आस्था, इस लोक के प्रति तीव्र विरक्ति, प्रबल त्याग-शक्ति एवं ईश्वर और अविनाशी आत्मा में दृढ़ विश्वास तुम लोगों में सतत् विद्यमान है। मैं किसी को भी चुनौती दे सकता हूँ कि इसे छोड़ का दिखाए? तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम कुछ महीनों भौतिकवादी बनकर और भौतिकवाद की चर्चा करके भले ही मुझ पर प्रभाव डालने की चेष्टा करो, पर मैं जानता हूँ कि तुम वास्तव में क्या हो। यदि मैं दुमका हाथ पकड़ कर ले जाऊँ, (तुमको थोड़ा धर्म अच्छी तरह समझा है। से बस, तुम पुनः हमेशा की भाँति परम् आस्तिक हो जाओगे। तुम अपना नैसर्गिक स्वभाव भला कैसे बदल सकते हो?
अतः भारत में किसी प्रकार के सुधार के लिए पहले धर्म में क्रांति लाने की आवश्यकता होती है। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। जिस कार्य पर हमें सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है वह है कि हमारे उपनिषदों, हमारे धर्मशास्त्रों, हमारे पुराणों में जो अपूर्व सत्य बंद पड़े हैं, उन्हें इन सब ग्रन्थों के पृष्ठों से बाहर निकालकर, मठों की चारदीवारियों से बाहर निकालकर, वनों की शून्यता से दूर लाकर, कुछ लोगों या मण्डलों के एकाधिकार से बाहर निकालकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा, ताकि ये सत्य दावानल के समान सारे देश को चारों ओर से लपेट लें - उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सब जगह फैल जाएँ - हिमालय से कन्याकुमारी तक और सिन्ध से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र वे धधक उठें।" (CWSV 3, 220-22)
प्रकृति के सभी गुण अपने सार-रूप में गुणात्मक हैं और इसी कारण वे उसके गुण कहलाते हैं। जगत् के विषय में किसी भी आध्यात्मिक परिकल्पना में ऐसा होना ही है; क्योंकि, आत्मा और जड़त्व को जोड़नेवाला माध्यम चैत्य या आत्म-शक्ति ही होनी चाहिए तथा प्रधान क्रिया मनोवैज्ञानिक अथवा आंतरिक एवं गुणात्मक होनी चाहिए, न कि भौतिक और मात्रात्मक; क्योंकि गुण विश्व-शक्ति के समस्त व्यापार में अभौतिक एवं अधिक आध्यात्मिक तत्त्व हैं, उसकी आदि गतिशक्ति हैं। भौतिक विज्ञान की प्रधानता ने हमें प्रकृति संबंधी एक भिन्न दृष्टिकोण का अभ्यस्त बना दिया है, क्योंकि वहाँ जो चीज हमें सबसे पहले प्रभावित करती है वह है उसकी क्रियाओं के परिमाणात्मक रूप का महत्त्व तथा आकारों के निर्माण के लिए मात्रात्मक सम्मिश्रणों एवं प्रबंधनों पर उसकी निर्भरता ।... प्राचीन भारतीय मनीषियों के विश्लेषण में प्रकृति की मात्रात्मक क्रिया, मात्रा, के लिए स्थान था; परंतु उसे इस रूप में माना जाता था कि वह तो प्रकृति की बाह्यतर और औपचारिक रूप से कार्य-निष्पादन की क्रिया का ही विशिष्ट धर्म है, जबकि सहज स्वरूप मात्र में ही उद्भावक (ideative) कार्यकर्ती-शक्ति, जो वस्तुओं का प्रबंधन उनकी सत्ता एवं शक्ति के धर्म, अर्थात् गुण एवं स्वभाव के अनुसार करती है, ही प्रधान निर्धारक शक्ति है और समस्त बाह्य मात्रात्मक प्रबंधनों के आधारस्वरूप स्थित रहती है। पर स्थूल जगत् के मूल में यह बात दृष्टिगोचर नहीं होती, केवल इस कारण कि यहाँ आधारस्वरूप उद्भावक आत्म-सत्ता, महत् भार जड़तत्व तथा जड़भौतिक शक्ति की गति के द्वारा आवृत्त एवं आच्छादित है। यदि कोई ऐसी श्रेष्ठतर शक्ति न हो जो वैविध्यकारक गुण से युक्त हो तथा जिसके ये भौतिक प्रबंधन केवल सुविधाजनक यांत्रिक साधनमात्र ही हों, तो इस स्थूल जगत् में भी एक-दूसरे के बिल्कुल ही समान तत्त्वों द्वारा उनके विभिन्न सम्मिश्रणों तथा मात्राओं के फलस्वरूप नानाविध अद्भुत परिणामों के उत्पन्न होने की बुद्धि से कल्पनीय कोई व्याख्या नहीं होगी। अथवा, हम एकाएक ही यों कह सकते हैं कि विश्व ऊर्जा की अवश्य ही एक निगूढ़ उद्भावक क्षमता, विज्ञान, है, भले ही हम स्वयं उस ऊर्जा तथा उसके सहायक या उपकरणीय भाव, बुद्धि, को उनकी अपनी प्रकृति में यांत्रिक मानें, – जो इन बाह्य प्रबंधनों की गणित को निर्धारित करती तथा उनके कार्यफलों को तय करती है: आत्मा के अंदर विद्यमान यह सर्वशक्तिमान विज्ञान ही इन साधनों को रचता और उपयोग करता है। और, प्राणिक तथा मानसिक सत्ता में तो गुण एकाएक ही स्पष्ट रूप से प्रधान शक्ति के रूप में दिखायी देता है, और ऊर्जा की मात्रा केवल एक गौण तत्त्व है। परन्तु वास्तव में मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक सत्ताएँ सभी गुण की निर्धारित-सौमाओं के अधीन हैं, यद्यपि जैसे-जैसे हम सत्ता की श्रृंखला में नीचे उतरते हैं वैसे-वैसे यह सत्य अधिकाधिक धूमिल होता दिखाई देता है। केवल आत्म-सत्ता हो, जो अपनी भाव-सत्ता एवं भाव-शक्ति, जिन्हें महत् और विज्ञान कहते हैं, के सामर्थ्य के द्वारा इन अवस्थाओं को स्थिर करती है, वह इस प्रकार से निधारित नहीं होती, गुण व मात्रा की किन्हीं भी सीमाओं के वशीभूत नहीं होतो, क्योंकि उसकी अमित और अनिर्धार्य अनंतता इन गुणों से श्रेष्ठतर है जिहें वह अपनी सृष्टि के लिए विकसित करती है और उनका उपयोग करती है।
यदि इसे सच्चे रूप से समझ लिया जाए तो संपूर्ण ब्रह्माण्ड के निर्माण का रहस्य पता लग जाता है। अपने कार्य के संपादन के लिए प्रकृति को जो भी आवश्यक लगता है वही प्रक्रिया अपना लेती है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बन जाता है जबकि दोनों ही घटकों में पानी के कोई भी गुण नहीं होते। प्रकृति की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि इस परिणाम के लिए उसे इसी प्रक्रिया का उपयोग करना पड़े परंतु जब तक उसके कार्य के लिए उसे सुविधाजनक प्रतीत होता है तब तक वह इसे प्रयोग करती है और जब उसे कुछ अन्य प्रक्रिया का प्रयोग करना हो तो कोई कारण नहीं है कि ऐसा वह न कर सके। अतः अपने आप में कोई कार्य-कारण नहीं है। किसी भी चीज का एकमात्र एक ही सच्चा कारण हो सकता है, और वह है जगज्जननी का संकल्प। उसकी पूर्ति के लिए वह जो चाहे वही प्रक्रिया अपना लेती है जो कि हमारी मानव बुद्धि को कार्य-कारण प्रतीत होता है। यदि बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो किसी समान ही कारण से भी भिन्न-भिन्त्र परिणाम उत्पन्न होते हैं।
इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह जगदंबा के संकल्प के द्वारा ही होता है। चूंकि हम वास्तविक कारण अर्थात् जगज्जननी के संकल्प को देख नहीं पाते इसलिए प्रक्रिया को ही हम कार्य-कारण मान बैठते हैं। इसी कारण यदि हम विज्ञान के दृष्टिकोण से जगत् का विश्लेषण करते हैं तो हमें कोई भी सच्चा परिदृश्य या चित्र प्राप्त नहीं होता क्योंकि विज्ञान तो मात्रात्मक है। उदाहरण के लिए, किसी भवन के निर्माण का कारण और उसका औचित्य यदि हम उसमें लगे इमारती सामान से करने लगें तो हमें कोई सच्ची सूचना कभी प्राप्त नहीं हो सकती। उसका सच्चा परिप्रेक्ष्य तो हमें केवल उसके मालिक के मन के विचार और उसकी रूपरेखा को जानकर ही पता लग सकता है। बाकी सभी ब्यौरे की सूचना भी तभी उपयोगी हो सकती है जब हमें उस परिप्रेक्ष्य का पता हो। अन्यथा तो यह अंधों के द्वारा किये हाथी के उस वर्णन के समान ही होगा जो समग्र हाथी को देखे बिना केवल उसके भिन्न-भिन्न अंगों का ही अपनी परोक्ष अनुभूति के अनुसार वर्णन करते हैं।
अतः मात्रात्मक रूप से नहीं अपितु गुणात्मक रूप से हम जगत् का अधिक सही वर्णन कर सकते हैं। यदि हम किसी प्रकार दिव्य जननी के संकल्प के प्रति सचेतन हो सकें तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार किसी कार्य की अभिव्यक्ति में मन, प्राण और शरीर का कितना-कितना योगदान होता है। अतः किसी भी कार्य के निष्पादन में तीनों ही गुण काम में आते हैं। केवल भारतीय संस्कृति में ही चीजों को इस रूप में देखा गया है, अन्य कहीं तो इसकी कल्पना तक भी नहीं रही है। अतः सभी कुछ का मूल कारण जगज्जननी का संकल्प है और अतिमानस उस संकल्प को चरितार्थ करता है। इस रूप से हम सृष्टि के सत्य को समझ सकते हैं। सारी अभिव्यक्ति भीतर से बाहर की ओर होती है न कि बाहर से भीतर की ओर। जबकि हमारा भौतिकवाद बाह्य प्रतीति को ही आधार मान बैठने की भूल कर बैठता है। इसीलिए सभी कुछ को अपने तरीके से समझाने के बाद भी वह वास्तव में किसी चीज का भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाता क्योंकि वास्तविक कारण तो जगदंबा का संकल्प ही है। यदि उस संकल्प में निहित प्रारूप को कोई थोड़ा-बहुत भी समझ सके तो वह सच्चे रूप से वस्तुओं के मूल कारण को कुछ-कुछ समझ सकता है। इसके अतिरिक्त इस जगत् के मूल कारण को समझने का कोई भी तरीका नहीं है। यहाँ तक कि किसी भवन का निर्माण भी किसी मूल विचार से आरंभ होता है और उसके बाद ही सारे साधन आदि जुटाए जाते हैं। परंतु जैसे कि हम उस मूल विचार के आधार पर ही निर्णय कर सकते हैं कि कौनसे साधन उस भवन के निर्माण के लिए आवश्यक है और कौनसे नहीं, उसी प्रकार जब हम उस मूल संकल्प में कुछ-कुछ प्रवेश कर सकें तब अभिव्यक्ति में उसकी क्रिया और प्रक्रिया को कुछ अधिक बेहतर ढंग से समझने लगते हैं।
हमारे पुराण आदि सृष्टि की इसी प्रक्रिया को अनेकों रूपकों के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकट करते हैं। पुराणों में हम पृथ्वी को तुलना शेषनाग के हजार फणों पर एक सरसों के दाने से की गई पाते हैं। आज का शिक्षित मनुष्य इसे एक बड़ी ही उर्वर कल्पना मानेगा और इसके विषय में हर कोई अपने-अपने तरीके के आक्षेप लगाएगा। परंतु जिन्हें कुछ गुह्य अनुभव है वे जानते हैं कि शेषनाग प्राणिक ऊर्जा का प्रतीक है। और भौतिक जगत्, जिसे कि सरसों के दाने के बराबर बताकर उसकी लघुता का आभास दिया गया है, अपने से उस अनंतगुना विशाल प्राणिक जगत् पर आधारित है। अतः प्राणिक जगत् की हलचल से हो यहाँ भौतिक जगत् में कोई भी हलचल होती है। यह एक बड़ा ही सटीक रूपक है परंतु केवल गहन अंतर्दृष्टि के द्वारा ही यह वास्तव में समझ में आ सकता है।
इस सारी चर्चा से हम गुणों और उनकी क्रियाओं को एक परिपेक्ष्य में देख सकते हैं। हालाँकि अन्य दृष्टिकोण भी हो सकते हैं परंतु इसके माध्यम से भी इस विषय में हमें कुछ बौद्धिक स्पष्टता आ जाती है।
परन्तु, दूसरी ओर, प्रकृति की संपूर्ण गुणात्मक क्रिया, जो अपनी बारीकियों तथा विविधताओं में अनंत रूप से जटिल है, इस प्रकार गोचर होती है कि वह गुण की इन तीन सर्वसाधारण अवस्थाओं', सत्त्व, रजस्, तमस्, के साँचे में हली है, जो कि सर्वत्र उपस्थित, परस्पर-गुँथे हुए और लगभग असमाधेय हैं। गीता में इन गुणों का वर्णन मनुष्य में होने वाली इनकी मनोवैज्ञानिक क्रिया के ही द्वारा किया गया है अथवा, प्रसंगवश, आहार आदि जैसी चीजों में भी उनका इस आधार पर वर्णन किया गया है कि वे मनुष्यों में किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक या प्राणिक प्रभाव डालते हैं। यदि हम इनकी अधिक व्यापक परिभाषा की खोज करें, तो....हम विश्व-ऊर्जा की गति के शब्दों में इन तीन गुणों या अवस्थाओं को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि ये प्रकृति की संतुलन, गतिक्रम और जड़ता की तीन सहचारी और अविभाज्य शक्तियाँ हैं। किन्तु यह तो ऊर्जा की बाह्य क्रिया की परिभाषा में इनकी केवल बाह्य प्रतीति है.... क्योंकि बाह्यतः निश्चेतन दिखनेवाली शक्ति में भी चेतना सदा ही विद्यमान रहती है, हमें इन तीन गुणों की उस तदनुरूप आंतरिक शक्ति का पता लगाना होगा जो इनकी अधिक बाह्य कार्यकारी क्रिया को अनुप्राणित करती है। अपने आंतरिक मनोवैज्ञानिक पक्ष में इन तीन गुणों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तमस् को प्रकृति की निर्ज्ञानता की शक्ति के रूप में, रजस् को उसकी कामना और प्रेरणा से आलोकित सक्रिय अन्वेषणशील अज्ञान की शक्ति के रूप में, सत्त्व को उसके अधिकृत और समन्वित करनेवाले ज्ञान की शक्ति के रूप में। प्रकृति की तीन गुणात्मक अवस्थाएँ समस्त जागतिक अस्तित्व में एक-दूसरी के साथ अविच्छेद्य रूप से गुँथी हुई हैं।
भगवान् के गुण तो अनंत हैं परंतु हमारी बाहरी सत्ता मन, प्राण और शरीरमय होने के कारण हमें ये गुण मोटे रूप से तीन तरीकों से प्रतीत होते हैं अन्यथा अपने-आप में तो कोई पृथक् चीज है नहीं कि एक को सत्त्व की, एक को रजस् की, और एक को तमस् की संज्ञा दे दी जाए। यह तो किसी नदी के प्रवाह की भाँति अटूट श्रृंखला है जिसका कोई विभागीकरण नहीं किया जा सकता। केवल मानसिक दृष्टिकोण से समझ सकने और उसकी चर्चा तथा व्याख्या आदि करने के उद्देश्य से ही हम उन्हें तीन मोटे विभागों में बाँट देते हैं। तीनों ही गुणों की अपनी-अपनी विस्तृत श्रृंखला है और प्रत्येक एक-दूसरे में घुला-मिला होता है।
_________________
* प्रकृति की तीन मूल अवस्थाओं का विचार प्राचीन भारतीय मनीषियों की उपज है और इसकी सत्यता हमारे सामने एकाएक ही स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि यह उनके सुदीर्घ अध्यात्मपरक परीक्षण तथा गंभीर आन्तरिक अनुभूति का परिणाम था। इसलिए, एक सुदीर्घ आन्तरिक अनुभव तथा अन्तरंग आत्म-निरीक्षण के बिना और प्रकृति शक्तियों के अंतर्ज्ञानात्मक बोध के बिना इसे ठीक-ठीक समझ पाना या सुदृढ़ रूप से उपयोग कर पाना कठिन है।
ये विभाग तो केवल बुद्धि की सुविधा के दृष्टिकोण से हैं अन्यथा तो कोई भी दो चीजें, कोई भी दो घटनाएँ एक समान नहीं होतीं। किसी एक व्यक्ति की तामसिक प्रकृति किसी दूसरे व्यक्ति की तामसिक प्रकृति से भी सर्वथा भिन्न होती है। स्वयं उस व्यक्ति-विशेष की प्रकृति में ही समय-समय पर अंतर आता रहता है।
[ये गुण] हमारी प्राकृत सत्ता के प्रत्येक भाग पर अपना प्रभाव डालते हैं। निःसन्देह इनका प्रबलतम सापेक्ष प्रभुत्व इसके तीन भिन्न अंगों अर्थात् मन, प्राण और शरीर पर होता है। तमस्, जो कि जड़ता का तत्त्व है, जड़ प्रकृति में तथा हमारी भौतिक सत्ता में सबसे अधिक प्रबल है। इस तत्त्व की क्रिया दो प्रकार की होती है, शक्ति की जड़ता और ज्ञान की जड़ता। जो कुछ भी प्रधान रूप से तमस् से शासित होता है उसकी शक्ति मन्द निष्क्रियता की ओर या फिर एक ऐसी यान्त्रिक क्रिया की ओर प्रवृत्त होती है जिस पर उसका नहीं अपितु अन्धकारमय शक्तियों का अधिकार होता है जो उसे ऊर्जा के यांत्रिक चक्र में चलाती रहती है।.... रजस्तत्त्व की प्रबलतम पकड़ प्राणिक प्रकृति पर रहती है। हमारे अन्दर का प्राणतत्त्व ही सबसे प्रबल एवं क्रियाशील चालक-शक्ति है, पर पार्थिव प्राणियों में प्राणिक शक्ति कामना-शक्ति के अधिकार में है। इसलिए रजस् सदा ही कर्म और कामना की ओर प्रवृत्त हो जाता है; कामना ही मनुष्य और पशु की अधिकांश गतिक्रम और क्रिया की प्रबलतम प्रवर्तिका है... यही नहीं, चूँकि रजस् अपने-आप को एक ऐसे जड़ भौतिक जगत् में पाता है, जो निश्चेतना तथा एक यांत्रिक रूप से चालित जड़त्व के तत्त्व से निकलता है, उसे एक अतिविशाल विपरीत शक्ति का सामना करते हुए अपना कार्य करना पड़ता है; अतएव, उसका सम्पूर्ण कार्य एक प्रयत्न का, एक संघर्ष का तथा अधिकार प्राप्ति के लिये एक ऐसे आक्रान्त एव बाधायुक्त संघर्ष का रूप ग्रहण कर लेता है जो अपने प्रत्येक पग पर एक सीमाकारी असमर्थता, निराशा और वेदना से व्यथित होता है: यहाँ तक कि उसे प्राप्त होनेवाली सफलताएँ भी अनिश्चित होती हैं, प्रयत्न की प्रतिक्रिया और उसके परिणामस्वरूप बाद में मिलने वाले अभाव और क्षणभंगुरता के स्वाद के द्वारा सीमाबद्ध और क्षत-विक्षत हो जाती हैं। सत्त्व के तत्त्व का प्रबलतम प्रभुत्व मन पर रहता है, मन के उन निम्नतर भागों पर तो उतना नहीं जो राजसिक प्राणशक्ति के द्वारा शासित हैं, पर अधिकांशतः बुद्धि तथा बुद्धिप्रधान संकल्प-शक्ति पर रहता है। बुद्धि, तर्कशक्ति तथा बौद्धिक संकल्पशक्ति अपने प्रधान तत्त्व (सत्त्वगुण) के स्वभाव के कारण समावेश करने या आत्मसात् करने की ओर, ज्ञान के द्वारा आत्मसात् करने तथा बुद्धिप्रधान संकल्प की शक्ति के द्वारा आत्मसात् करने की ओर, प्रवृत्त होते हैं, (साथ ही) एक सन्तुलन स्थापित करने, किसी प्रकार की स्थिरता एवं कोई नियम स्थापित करने और स्वाभाविक घटना एवं अनुभूति के परस्पर विरोधी तत्त्वों के सामंजस्य को प्राप्त करने के लिये अनवरत यत्न करने में भी प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार की तुष्टि को सत्त्वगुण नानाविध प्रकारों से तथा तुष्टि-प्राप्ति की नानाविध मात्राओं में प्राप्त करता है। आत्मसात्करण, सन्तुलन और सामंजस्य की प्राप्ति अपने साथ सदा ही सुख, प्रसन्नता, प्रभुत्व और सुरक्षा की एक सापेक्ष, पर न्यूनाधिक तीव्र एवं तुष्टिकारक अनुभूति ले आती है, जो कि राजसिक कामना और आवेग की तुष्टि के द्वारा असुरक्षित रूप में प्राप्त होनेवाले अशान्त एवं उग्र सुखों से भिन्न प्रकार की होती है। प्रकाश और प्रसन्नता सत्त्वगुण के विशिष्ट लक्षण हैं। देहधारी प्राणवंत मनोमय प्राणी की सम्पूर्ण प्रकृति इन तीन गुणों के द्वारा निर्धारित होती है।
तमस् जड़ता का तत्त्व है। इसके प्रभाव से व्यक्ति में अंधकारमय शक्तियों का प्रभुत्व रहता है जो उसे यंत्रवत् चलाती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति कोई महत् कार्य करने की नहीं सोचता। वह अपने जीवन के ढरें में किसी यंत्र की भाँति चलता रहता है और किसी भी परिवर्तन का सहज ही विरोध करता है। परंतु गतिशील और ऊर्जस्वी प्रकृति होने के कारण हमारी प्राणिक सत्ता को इस निष्क्रियता की प्रवृत्ति द्वारा प्रस्तुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्राण की जो भी कामनाएँ, इच्छाएँ, आवेग, महत्त्वाकाक्षाएँ, लालसाएँ आदि हैं, उन सभी को पूरा करने में मनुष्य को घोर परिश्रम करना पड़ता है। यह एक आम बात है कि जिसने भी अपने समक्ष कोई बड़ा लक्ष्य रखा है उसे संसिद्ध करने में उसे स्वयं अपनी और सामूहिक जड़प्रकृति के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि अपने दैनंदिन जीवन और अपने परिवार को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को अथक परिश्रम करते रहना पड़ता है अन्यथा तो वह सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता। इसी को हमारे पुराणों में गज और ग्राह के रूपक के द्वारा समझाया गया है। हमारी जड़भौतिक प्रकृति ग्राह है और प्राणिक प्रकृति गज है। अतः जड़भौतिक के सामने प्राणिक प्रकृति की एक नहीं चलती। इसके लिए जब प्राणिक प्रकृति मन पर अपना प्रभाव डालकर उसे अपने अधीन कर लेती है तय उसकी सहायता से वह भौतिक पर आधिपत्य करती है। इसीलिए संसार में जिनमें प्राण की प्रधानता है और मानसिकता विकसित होती है वे ही दूसरों पर आधिपत्य करते हैं। जिनमें केवल बौद्धिकता विकसित होती है परंतु प्राण निर्बल होता है ऐसे व्यक्ति कुछ भी चरितार्थ नहीं कर पाते। जिनमें प्राण प्रधान हो परंतु बुद्धि न हो तो वे सदा ही दिग्भ्रमित रहते हैं और किसी सही दिशा में गति नहीं कर पाते। इसलिए जिन्होंने भी महान कृतियाँ या कृत्य किये हैं वे सभी ऐसे लोग हैं जिनमें प्राण प्रधान रहा है और बौद्धिकता विकसित रही है। परंतु यह सब होने पर भी ऐसे लोगों को भी अंततः जड़त्व अपने अधिकार में लेकर उन्हें नष्ट कर देता है। इसलिए संपूर्ण जीवन संघर्षमय ही रहता है क्योंकि रजस् को एक ऐसे जड़तत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जिससे वह अंततः जीत नहीं सकता।
जब हम इन गुणों की क्रिया को समझ जाते हैं तब हम सामाजिक व्यवस्था में इनके प्रभाव को भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। जिनमें प्राण प्रधान हो और मन उसकी सेवा में तत्पर हो ऐसे लोगों को यदि हम भेड़ियों की संज्ञा दें और जिनमें जड़त्व प्रधान हो उन्हें भेड़ों की संज्ञा दें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज में भले ही बाहुल्य तमस् प्रधान व्यक्तियों का ही है जो केवल अपने-आप की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में और अधिक से अधिक क्षुद्र राजसिक वृत्तियों की पूर्ति में लगे रहते हैं परंतु फिर भी जैसे सैंकड़ों भेड़ें मिल कर भी किसी एक भेड़िये का सामना नहीं कर सकतीं उसी प्रकार भले शासन व्यवस्था कोई भी क्यों न हो, परंतु शासन तो केवल सदा ही मन द्वारा समर्थित प्राण प्रधान लोग ही करते हैं। इसलिए जब तक हम इस मूल तथ्य को नहीं समझ लेते तब तक कोई भी सुशासन संभव ही नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का आदर्श प्रदान किया। परंतु सच्ची समानता और स्वतंत्रता केवल भ्रातृत्व के आधार पर ही स्थापित हो सकती है। और जब तक अहं का शासन है तब तक सच्चा भ्रातृत्व स्थापित नहीं हो सकता क्योंकि भ्रातृभाव तो आत्मा का गुण है। किसी परिवार में भ्रातृभाव के कारण ही सभी को समान ही प्रेम का व्यवहार प्राप्त होता है चाहे उन सब में कितनी भी भिन्नताएँ, क्षमताएँ-अक्षमताएँ आदि क्यों न हो। एतु यदि इस समन्वयकारी भाव को हटा लिया जाए तो वही परिवार कुछ ही समय में कलहरत होकर बिखर जाता है। केवल भ्रातृभाव के कारण हो परिवार में किसी एक की उन्नति के कारण सभी को सुख मिलता है और किसी एक की अक्षमता की पूर्ति करने और उसकी सहायता करने के लिए सभी तत्पर रहते हैं। हालाँकि एक सीमा के बाद बाहरी भ्रातृभाव तो टूट सकता है, परंतु आत्मा में निहित सच्चा भ्रातृभाव अटूट रहता है और किन्हीं भी परिस्थितियों में अडिग बना रहता है। इसलिए मनुष्यजाति को यदि कलह से मुक्त करना है और एकता के सूत्र में पिरोना है तो आत्मा में स्थित इस भ्रातृभाव को सामने लाना होगा। यदि सच्चे रूप से यह भाव सामने आ जाए तो किसी भी बाहरी नियम-विधान की कोई आवश्यकता नहीं होगी और केवल तभी यह भेड़ और भेड़िये के अंतर को मिटाया जा सकता है, अन्य किसी भी उपाय से नहीं। और सारी मनुष्यजाति के समक्ष आत्मा में निहित इस भ्रातृत्व को प्रकट करना, इसका पाठ पढ़ाना भारत के लिये भगवत्प्रदत्त कार्य रहा है। इसलिए मनुष्यजाति का भविष्य भारत के उत्थान पर निर्भर करता है क्योंकि किन्हीं दिशाओं में अवश्य ही मानव ने अत्यधिक प्रगति कर ली है जबकि उसका उपयोग करने वाली चेतना अभी भी अहंमय ही बनी हुई है। इसलिए जिस संकटकाल में मनुष्यजाति वर्तमान में खड़ी है उसमें उसके चयन पर निर्भर करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। यदि वह बेरोकटोक इसी तरह अपने स्वार्थों की पूर्ति करने की दिशा में ही गति करती रहे तो इसका विनाश निश्चित है। इसलिए वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आत्मा पर आधारित यह भ्रातृत्व स्थापित नहीं होता और अंधे स्वार्थ पर लगाम नहीं लगा देता तो यह सारी मनुष्यजाति के लिए एक घातक स्थिति होगी।
प्रश्न : परंतु वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए क्या ऐसी कोई संभावना नजर आती है कि आत्मा का यह गुण - भ्रातृत्व - स्थापित हो सके, क्योंकि चारों ओर हम मिथ्यात्व, वैमनस्य, स्वार्थपरता और घोर अंधकार का ही बोलबाला देखते हैं?
उत्तर : अतीत में ऐसे काल और ऐसी सभ्यताएँ रह चुकी हैं जहाँ बहुत सामंजस्य था। इसलिए यदि हम केवल प्रतीतियों से ही भ्रमित होकर न देखें और यह मानकर चलें कि प्रकृति में उत्तरोत्तर विकास ही हुआ है न कि अवनति, और फिर आज हमारे पास पहले से अधिक साधन हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह न किया जा सके। हमारे प्राचीन ऋषि, जिन्होंने समय-समय पर स्वयं आकर सदा ही मनुष्यजाति को आगे बढ़ाया है, वे अब भी प्रकट अथवा सूक्ष्म तरीकों से आध्यात्मिक सत्य को हमारे स्थूल से स्थूल भागों में भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज को हमारे स्थधक साधन इतने तीव्र हो चुके हैं कि किसी एक स्थान पर हुई प्रचार आप बहुत थोड़े ही समय में विश्व भर में फैल जाती है। जब कोई उपलबिल आदि के साधन नहीं थे तब भी स्वयं शंकराचार्य ने सोलह वर्षों की अल्पायु में ही सारे भारत का भ्रमण कर हिन्दू धर्म का प्रचार-प्रसार कर दिया था तथा मठों का निर्माण कर दिया था। आज जब हम तकनीकी की दृष्टि से कहीं अधिक साधन संपन्न हैं तो एक बार कहीं आत्मा का प्रकाश प्रस्फुटित होता है उसे सभी जगह फैलाने में तो अधिक समय नहीं लगेगा। आत्मा की शक्ति अप्रतिरोध्य और अमोघ होती है। इसीलिए गौतम बुद्ध जिस किसी मार्ग से निकलते थे वहीं सभी अपने आप ही बौद्ध धर्म अपना लेते थे। अतः जब आत्मा की शक्ति प्रकट होती है तब उसमें अदम्य शक्ति होती है और वह चाहे जो चीज चरितार्थ कर सकती है। हमारे अपने समय में हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देख सकते हैं। कितने थोड़े ही काल में उन्होंने विश्व भर में 'कृष्ण चेतना' का प्रचार प्रसार कर दिया जबकि न तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य ही अच्छा था और न ही उनके पास कोई विशेष संसाधन थे। परंतु फिर भी चूंकि उन्हें अपने भीतर से यह आदेश प्राप्त था कि उन्हें यह प्रचार-प्रसार करना है इसलिए उन्होंने निष्ठापूर्वक उसका पालन किया और आज विश्व भर में हम उसकी जीवंत चरितार्थता देख सकते हैं और जबकि स्वयं प्रभुपाद जी आज शरीर में नहीं हैं, तो भी भक्तों की अधिकाधिक संख्या नित्यप्रति उस ओर आकर्षित हो रही है और इससे लाभान्वित हो रही है। अतः यदि किसी प्रकार आत्मा का सच्चा प्रकाश आ सके तो विश्व भर में उसे फैलने में और पूरे परिदृश्य को ही बदल डालने में अधिक समय नहीं लगेगा।
परन्तु हमारी सत्ता के जटिल तंत्र के प्रत्येक भाग में ये केवल प्रधान शक्तियाँ ही हैं। ये तीनों गुण हमारे पेचीदा मनोविज्ञान के प्रत्येक तन्तु एवं प्रत्येक अंग में घुल-मिलते, संयुक्त होते तथा कलह करते हैं। हमारा मानामिक स्वरूप, हमारी बुद्धि का स्वरूप, संकल्पशक्ति का स्वरूप, हमारी नैतिक, गुणों के द्वारा ही निर्मित होता है। तमस् उस समस्त अज्ञानता, जड़ता, दुर्बलता एवं असमर्थता को ले आता है जो हमारी प्रकृति को पीड़ित करती है, और साथ ही ले आता है तमसाच्छन्न बुद्धि, निर्जान, अबुद्धि, अफरती धारणाओं और यान्त्रिक विचारों के प्रति आसक्ति, विचारने और जानने से इन्कार करने की वृत्ति को, संकुचित मन को, बन्द मार्गों को, मानसिक आदत के चक्कर काटते रहने को और अन्धकारमय एवं धूमिल स्थान को। तमस् ले आता है अशक्त संकल्पशक्ति को, श्रद्धा, आत्म-विश्वास और नए अभियानों को आरंभ करने के उत्साह के अभाव को, क्रिया करने में अरुचि को, उद्यम और अभीप्सा से कतराने की वृत्ति को, तुच्छ और क्षुद्र भाव को, और हमारी नैतिक और क्रियाशील सत्ता में वह ले आता है निष्क्रियता अथवा जड़ता, भीरुता, नीचता, मंदता, तुच्छ और हीन हेतुओं के प्रति शिथिल अधीनता, अपनी निम्न प्रकृति के प्रति दुर्बलतापूर्ण वश्यता को। हमारी भावप्रधान प्रकृति में तमस् ले आता है सम्वेदनहीनता, उदासीनता, सहानुभूति एवं ग्रहणशीलता के अभाव को, बन्द आत्मा एवं क्रूर हृदय को, शीघ्र थक जानेवाले अनुराग और भावनाओं की मन्दता को, हमारी सौन्दर्यात्मक और सम्वेदन-प्रधान प्रकृति में वह सौन्दर्यवृत्ति की जड़ता, प्रतिक्रिया-शक्ति की परिमितता एवं सौन्दर्य के प्रति सम्वेदनहीनता को तथा उन सब चीजों को जो मनुष्य में स्थूल, तामसिक और असंस्कृत भाव को उत्पन्न करती हैं। रजस् हमारी सामान्य सक्रिय प्रकृति को अपनी सभी भली और बुरी वृत्तियाँ प्रदान करता है; जब वह सत्त्वगुण के पर्याप्त अंश के द्वारा अभी विशुद्ध नहीं हुआ होता तब वह अहंकार, स्वेच्छाचारिता और उग्रता, बुद्धि की विकृत, हठी या अतिरंजक क्रिया, पूर्वाग्रह, अपने मत के प्रति आसक्ति, भूल से चिपके रहने की वृत्ति, सत्य के प्रति नहीं अपितु हमारी कामनाओं एवं अभिरुचियों के प्रति बुद्धि की अधीनता, धर्मान्ध या कट्टरपंथी मन, हठधर्मिता, गर्व, अभिमान, स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा, काम-वासना, लोभ, क्रूरता, घृणा, ईर्ष्या, नाना प्रकार के प्रेममूलक अहंकार, समस्त पाप और वासनाएँ, सौन्दर्यबोध की अतिरंजनाएँ, सम्वेदनात्मक और प्राणिक सत्ता की व्याधियाँ और विकृतियाँ - इन सभी की ओर प्रवृत्ति रखता है। अपने निज अधिकार में तमस् असंस्कृत, जड़ और अज्ञानमय प्रकार की मानव प्रकृति को जन्म देता है, रजस् कर्म, आवेश और कामना के भाव से चालित, प्राणवन्त, चंचल एवं क्रियाशील मानव को जन्म देता है। सत्त्व एक उच्चतर कोटि के मानव को जन्म देता है। सत्त्वगुण की देनें हैं - विवेकशील और सन्तुलित मन, निष्पक्ष, सत्यान्वेषिणी एवं ग्रहणशील बुद्धि की बोधगम्यता, बुद्धि के अधीन या नैतिक भाव के द्वारा परिचालित संकल्पशक्ति, आत्म-संयम, समता, शांत-स्थिरता, प्रेम, सहानुभूति, शिकता संकल्पात सोन्दर्ययाही और भावमय मंत्र की सूक्ष्मता, सम्वेदनात्मक राजा है सुकोमलता, समुचित ग्रहणशीलता, मितव्यवहार और संतुलन, प्रभुत्व बुद्धि के वश में रहनेवाली और उसके द्वारा परिचालित प्राणशक्ति। याचिक अविध के सिद्ध प्रकार या उदाहरण हैं दार्शनिक, सन्त और ज्ञानी यान्ति, राजसिक मनुष्य के सिद्ध उदाहरण हैं राजनीतिज्ञ, योद्धा और शक्तिशाल कर्मवीर। परन्तु सभी मनुष्यों में गुणों का कम या अधिक अनुपात में परमार सम्मिश्रण पाया जाता है, बहुविध व्यक्तित्व देखने में आता है और अधिकार में तो काफी परिवर्तन एवं किसी एक गुण के प्रभुत्व से दूसरे गुण का प्राधान प्रतिस्थापित होता रहता है; यहाँ तक कि उनकी प्रकृति के किसी प्रधान गु द्वारा शासित होने पर भी अधिकांश मानव एक मिले-जुले प्रकार के होते हैं जीवन के सभी रंग और विविधता इन गुणों की बुनावट की जटिल बनावट में बने हैं।
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसक्नेन चानघ ।। ६।।
६. हे निष्पाप! इन गुणों में से सत्त्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरोगता देनेवाला है; यह सुख के तथा ज्ञान के साथ आसक्ति के द्वारा बाँषता है।
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ।। ७।।
७. हे कौन्तेय! रजोगुण को तू रागात्मक (आकर्षणात्मक) स्वभाव वाला जान; कामना और आसक्ति से उत्पन्न होने के कारण यह देहधारी जीव को कमाँ के साथ आसक्ति के द्वारा बाँधता है।
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ।। ८।।
८. और अज्ञान से उत्पन्न हुए तमस् को तू समस्त देहधारी जीवों को गोविन करने वाला जान; हे भारता वह प्रम को तो समस्त देहधारी कीबात का को बाँधता है।
सत्त्व सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ।। ९।।
९. हे भारत! सत्त्वगुण मनुष्य को सुख में आसक्त करता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके मनुष्य को प्रमाद में आसक्त करता है।
गीता कहती है कि "प्रकृति से उत्पन्न ये तीन गुण देह के अंदर निवास करनेवाले अविनश्वर देही को देह में बाँध देते हैं।" इसका कारण... है गुणों तथा उनकी क्रियाओं के परिणामों के प्रति हमारी आसक्ति। सत्त्व... सुख-प्रसन्नता में आसक्त करता है, रजस् कर्म में आसक्त करता है और तमस् ज्ञान को आच्छादित कर देता है और भूल-भ्रांति एवं अकर्मरूपी प्रमाद में आसक्त कर देता है।.... दूसरे शब्दों में, जीव गुणों तथा उनके परिणामों के उपभोग के प्रति आसक्ति के द्वारा अपनी चेतना को प्रकृति में मन-प्राण-शरीर की निम्नतर एवं बाह्य क्रिया-व्यवहार पर केंद्रित करता है, इन वस्तुओं के बाह्य रूप के अंदर अपने को कैद कर देता है और (अपनी स्थूल सत्ता के) पीछे की ओर आत्मा के अंदर अवस्थित अपनी स्वयं की महत्तर चेतना को भूल जाता है, मोक्षदायी 'पुरुष' की स्वतंत्र शक्ति एवं विस्तार-क्षेत्र से अनभिज्ञ रहता है। अतः यह स्पष्ट ही है कि मुक्त और पूर्ण होने के लिए हमें इन चीजों से पीछे हटना होगा, गुणों से विलग होकर उनके ऊपर उठना होगा और प्रकृति के ऊपर अधिष्ठित उस मुक्त अध्यात्म-चेतना की शक्ति तक पुनः जाना होगा।
अतः यह निश्चित है कि ये तीनों ही गुण व्यक्ति को आत्म-विस्मृति कराते हैं और विश्व-प्रपंच में आसक्त कर देते हैं। तमस् सुख और निष्क्रियता में आसक्त करता है, रजस् कर्म और गतिशीलता में आसक्त करता है और सत्त्व ज्ञान में आसक्त करता है। तीनों ही अपने-अपने तरीके से व्यक्ति को आसक्त करते हैं और आंतरिक सत्ता के प्रति विस्मृति लाते हैं। इसीलिए परंपरा से ही इसका प्रचलित उपाय रहा है अक्षर ब्रह्म में अपने आप को स्थित कर लेना और गुणों की क्रिया को अपने हाल पर छोड़ देना। परंतु यह तो आरोहण में पहला पड़ाव मात्र ही हो सकता है। ये निर्लिप्तता या उदासीनता पूर्णत्व की स्थिति नहीं हैं। तो भी, आत्मा के विकास की किसी अवस्था विशेष में, जब व्यक्ति बाहरी चीजों में, संबंधों आदि में अतिशय रूप से आसक्त होता है, यह भाव लाभकारी हो सकता है। अक्षर ब्रह्म के प्रभाव से जब व्यक्ति साक्षी भाव का अभ्यास करता है तब उसे इन अतिशय बाह्य आसक्तियों के ज्वर से कुछ राहत अवश्य मिलती है और वह किसी श्रेष्ठतर चीज के विषय में सोचने-समझने की स्थिति में आता है अन्यथा तो वह इन आसक्तियों से ही इतना अभिभूत और पीड़ित रहता है और इन्हीं के द्वारा रात-दिन यंत्रवत् चलाया जाता है और किसी श्रेष्ठ आदर्श के विषय में तो उसे सोचने का अवकाश ही नहीं होता। इसलिए ये निर्लिप्तता आदि आसक्ति की पीड़ा से निवृत्त करने में तो सहायक हैं परंतु इनका अन्य कोई सकारात्मक उपयोग कम ही है।
प्रश्न : ज्ञान की आसक्ति का क्या अर्थ है? क्या ज्ञान में भी आसक्ति हो सकती है?
उत्तर : ज्ञान का निश्चय ही अपना एक आकर्षण होता है जिससे छूट निकलना राजसिक लालसाओं और तामसिक वृत्तियों से भी कहीं अधिक दुष्कर है क्योंकि तामसिक और राजसिक वृत्तियों में तो कहीं न कहीं व्यक्ति को अपने बंधन का तथा अपने गलत होने का आभास हो सकता है परंतु ज्ञान के अंदर तो व्यक्ति अपने को इतना परिपूर्ण अनुभव करता है कि उसे तो वह छोड़ना ही नहीं चाहता। इसलिए श्रीअरविन्द कहते हैं कि, "चाहे हम एकांगी रूप से 'विद्या' का अनुगमन करें या 'अविद्या' का, दोनों हालातों में ही हम समान रूप से पथभ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि एकांगिता का अर्थ है अज्ञान, एकांगिता का अर्थ है विभ्रम तथा अविभाज्य ब्रह्म का विभाजन। और ऐसी त्रुटि में दृढ़ संलग्नता एक ऐसा हठ है जो आत्मा की उसकी निकटतम संभावनों के लिए घातक है। यद्यपि शाश्वत काल के लिए नरकवास तो संभव नहीं है परंतु फिर भी कुछ काल के लिए मृत्यु को सफलतापूर्वक पार करने में वह विफल होता है और (त्रिशंकुवत्) अर्ध-मर्त्य (trans-mortal) अंधकार में प्रवेश कर जाता है। वे लोग पूर्णता-प्राप्त करते हैं, सिद्ध होते हैं जो ब्रह्म को एकात्मकता को स्वीकार करते हैं, जो विद्या और अविद्या दोनों में केवल व्यवहार देखते हैं, प्रकाश और अंधकार को 'उसमें' प्रतिबिंबित देखते हैं जो दृश्य-जगत् में केवल आत्म-अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए गए हैं. जो 'अनेकात्मक' में एकमेव के होने के ज्ञान में निवास करते हैं, जो सभो को ब्रह्मस्वरूप या ब्रह्मभाव में आलिंगन करते हैं, जो कुछ भी अस्वीकार नहीं करते, कुछ भी अभिरुचि नहीं रखते, सभी कुछ सहन अथवा वहन करते हैं, सभी कुछ संपन्न करते हैं, त्याग के द्वारा अनंत शांतिसंपन्न हैं, हर्ष के द्वारा अनंत शक्ति और आनंदयुक्त हैं।"* अतः अपनी सच्ची स्थिति में आत्मा विद्या और अविद्या दोनों का समान ही रूप से उपयोग कर सकती है। इसी प्रकार आत्मा के लिए जन्म और मृत्यु भी घटनाएँ मात्र ही हैं। यह न तो जन्म से बंधी होती है और न ही मृत्यु से, वह इनसे परे होती है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए वह इन दोनों को समान ही रूप से उपयोग में ला सकती है। परमात्मा की चेतना हमारी किन्हीं भी परिकल्पनाओं से सर्वथा परे है। इसलिए वह चेतना हम जिसे शुभ कहते हैं उसे भी उतना ही अपने उपयोग में ले लेती है जितना कि उसे जिसे हम अशुभ कहते हैं। क्योंकि यह सारी शब्दावली तो मनुष्य की रची हुई है जबकि परमात्मा अपनी क्रिया के लिए हमारी किन्हीं भी शब्दावलियों से बाध्य नहीं हैं। वे मुक्त रूप से अपनी क्रिया करते हैं। और उस क्रिया में कुछ चीजें हमारी शब्दावली के अनुसार शुभ के दायरे में आ सकती हैं और कुछ अशुभ के। परंतु परमात्मा की चेतना में ऐसा कोई विभेद नहीं है। वे हमारी किन्हीं भी मानसिक परिभाषाओं से सर्वथा परे हैं।
___________
* CWSA 17, p. 387
रजस्तमश्वाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ।। १० ।।
१०. हे भारत! कभी सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण सत्त्वगुण और तमोगुण को दबाकर प्रधान हो जाता है और कभी तमोगुण सत्त्वगुण और रजोगुण को दबाकर प्रधान हो जाता है।
प्रकृति के ये तीन गुण सभी मनुष्यों में स्पष्टतः ही विद्यमान और सक्रिय हैं और किसी को भी इनमें से किसी एक या दूसरे से सर्वथा रहित या तीनों में से किसी एक से विमुक्त नहीं कहा जा सकता; कोई भी व्यक्ति अन्य गुणों के बिना केवल एक ही गुण के साँचे में ढला हुआ नहीं है। सभी लोगों के अंदर कामना और कर्म का राजसिक आवेग किसी-न-किसी मात्रा में विद्यमान है और साथ ही प्रकाश एवं सुख-प्रसन्नता का सात्त्विक वरदान, कुछ संतुलन, अपने-आप के, अपनी परिस्थितियों तथा अपने विषयों के प्रति मन का कुछ सामंजस्य भी सबको प्राप्त है, और सभी को तामसिक अशक्तता, अज्ञान या निश्चेतना का अपना-अपना भाग भी मिला हुआ है। परंतु ये गुण अपनी शक्ति की मात्रात्मक क्रिया में या अपने तत्त्वों के संयोग में किसी भी मनुष्य के अंदर स्थिर रूप में विद्यमान नहीं हैं; क्योंकि ये परिवर्तनशील हैं तथा निरंतर, ही आपसी टक्कर, स्थान-परिवर्तन तथा पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया की अवस्था में रहते हैं। कभी तो एक नेतृत्व करता है और कभी दूसरा प्रबल हो जाता तथा प्रधानता प्राप्त कर लेता है, और प्रत्येक हमें अपनी विशिष्ट क्रिया तथा उसके परिणामों के अधीन कर देता है। किसी एक या दूसरे गुण की एक व्यापक तथा साधारण रूप से प्रमुखता के द्वारा ही किसी मनुष्य को उसकी प्रकृति में सात्विक या राजसिक या तामसिक कहा जा सकता है, पर यह तो केवल एक सामान्य लक्षण हो सकता है, न कि कोई अनन्य या चरम लक्षण। ये तीन गुण त्रिविध शक्ति हैं और अपनी क्रिया-प्रतिक्रिया के द्वारा ये प्राकृतिक मनुष्य के चरित्र एवं स्वभाव का निर्धारण करते हैं तथा उस स्वभाव के और उसकी विविध चेष्टाओं के द्वारा मनुष्य के कार्यों का भी निर्धारण करते हैं।
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।। ११ ।।
११. जब इस देह के समस्त द्वारों से ज्ञान का आलोक प्रकाशित होता है, तब ऐसा जानना चाहिए कि सत्त्वगुण की वृद्धि हुई है।
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ।। १२ ।।
१२. हे भरतश्रेष्ठ अर्जुना लोभ, प्रयत्नशीलता, कर्मों का अनुष्ठान, व्याकुलता और कामना-लालसा, ये सब रजोगुण की वृद्धि होने पर प्रकट होते हैं।
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह एव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।। १३।।
१३. हे कुरुनन्दन! अंधकार, अकर्मण्यता, प्रमाद और मोह (संभ्रम) ये सब तमोगुण की वृद्धि होने पर प्रकट होते हैं।
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ।। १४।।॥
१४. जब देहधारी जीव सत्त्वगुण की प्रधानता की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह सर्वोच्च के ज्ञाता व्यक्तियों के योग्य निर्मल लोकों को प्रात होता है।
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ।। १५।।
१५. रजोगुण की प्रधानता की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करके मनुष्य ऐसे मनुष्यों के मध्य जन्म ग्रहण करता है जो कर्म में आसक्त होते हैं; और तमोगुण की प्रधानता की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करके वह अविद्या-अंधकार में लीन जीवों की योनियों में उत्पन्न होता है।
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ।। १६ ।।
१६. समुचित रूप से किये गए कर्मों का फल शुद्ध और सात्त्विक कहा जाता है; राजसिक कर्मों का फल दुःख और तामसिक कर्मों का फल अज्ञान कहा जाता है।
---------------------------
* सत्त्व आदि प्रधान गुण देहधारी जीव के मूल आत्मिक प्रतिरूप नहीं होते, वरन उब रचना के चिह्न मात्र होते हैं जो रचना जीव अपने इस जीवन के लिये या अपने वर्तमान सत्ता-काल में अपने विकास के किसी विशिष्ट क्षण में निर्मित करता है।
सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।। १७॥
१७. सत्त्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ; तमोगुण से प्रमाद, मोह, और साथ ही अज्ञान भी, उत्पन्न होते हैं।
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥
१८. जो सत्त्वगुण में स्थित हैं वे ऊपर की ओर गति करते हैं, जो रजोगुण में स्थित हैं वे मध्य में बने रहते हैं; और जो तमोगुण में स्थित हैं वे, निकृष्टतम गुण की प्रवृत्तियों में रहने के कारण, नीचे की ओर जाते हैं।
सामान्य मानव जीव अपने प्राकृत-जीवन के चिर-अभ्यस्त विक्षोभों में एक तरह का सुख लेता रहता है; और चूँकि उसे उनमें सुख मिलता है और इस सुख से सुखी होकर वह निम्न प्रकृति की अशांत क्रीड़ा को अपनी अनुमति देता है इसलिए त्रिगुणात्मिका प्रकृति की यह क्रीड़ा सदा चलतो रहती है; क्योंकि प्रकृति अपने प्रेमी और भोक्ता पुरुष के सुख के लिए ही और उसकी अनुमति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करती।... हमारे राजसिक कामनामय पुरुष के लिए एकरस सुख, संघर्षरहित सफलता और छाया रहित हर्ष कुछ काल बाद अवसादकर, नीरस, और अतृप्तिकर होने लगता है, प्रकाश के उपभोग को पूरा मूल्य प्रदान करने के लिए इसे अंधकार को एक पृष्ठभूमि चाहिएः क्योंकि जो सुख वह चाहता और भोगता है वह ठीक उसी स्वभाव का है, वह अपने तत्त्वमात्र में सापेक्ष होता है और अपने विपरीत तत्त्व के बोध और अनुभव पर निर्भर है। आत्मा को जगत् के द्वंद्वों में मिलने वाला आनंद ही मन को जीवन से मिलने वाले सुख का रहस्य है।
हमारे जीवन में अधिकांश समस्याओं का कारण हमारा राजसिक कामनामय पुरुष है। यदि जीवन में एकरसता हो, चीजें सुचारू रूप से चल रही हों, किसी प्रकार का कोई कलह आदि न हो, किसी प्रकार का दुःख, वियोग न हो, तीव्र हर्ष और शोक न हो तो वह ऊब जाता है। अपने मन बहलाव के लिए नित्य प्रति वह नई-नई चीजें ढूँढ़ने में लगा होता है। वह किसी तीव्र सुख में भी उतना ही पुष्ट होता है जितना कि किसी तीव्र पीड़ा में, किसी यंत्रणा में। इसलिए जो प्राण प्रधान लोग होते हैं वे सदा ही कलहरत दिखाई देते हैं क्योंकि प्राणिक प्रकृति उन्हें वैसा करने को बाध्य करती है। हमारी प्राणिक प्रकृति को यह कहने में बहुत सुख अनुभव होता है कि जीवन में उसने सब के साथ भला किया है जबकि उसके साथ सदा ही अन्याय, अत्याचार और धोखा ही हुआ है। प्रायः ही हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि व्यक्ति ने आवश्यकता या संकट के समय अपने किसी मित्र या अपने सगे संबंधियों की भरसक सहायता की परंतु उन्होंने कभी उसके प्रति किसी प्रकार की कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं की और न ही जब स्वयं उसे सहायता की आवश्यकता थी उस समय किसी प्रकार की कोई सहायता ही प्रदान की। ऐसे ही अनेक तरीकों से प्राणिक प्रकृति अपने आप का गुणगान करके, अपना महिमा मण्डन कर के तुष्टि बटोरने का प्रयास करती है।
यदि इस मन से इन सब विक्षोभों से ऊपर उठने और उस विशुद्ध आनन्दमय पुरुष के अमिश्र सुख को प्राप्त करने के लिए कहा जाए जो सब गुप्त रूप से जीवन को उसके संघर्ष में सहारा देता है और उसकी सत्ता को निरंतर बनाए रखना संभव बनाता है, तो वह तुरन्त इस माँग से घबराकर पोछे हट जाएगा।.... मन की अनिच्छा का वास्तविक कारण यह है कि उससे अपने निजी वातावरण से ऊपर उठने और जीवन की एक अधिक असाधारण और अधिक विशुद्ध वायु का सेवन करने के लिए कहा जाता है, जिसके आनन्द और शक्ति को वह अनुभव नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि उसको वास्तविकता पर भी मुश्किल से ही विश्वास करता है, जबकि इस निम्नतर गँदली प्रकृति के सुख ही इसके लिए एकमात्र परिचित और स्पर्शगोबर या भोग्य है। और न ही यह निम्नतर तुष्टि अपने-आप में कोई दोषपूर्ण जा निरर्थक चीज ही है; अपितु यह तो अन्नमय पुरुष जिस तामसिक अज्ञान और जड़त्व के अत्यंत अधीन होता है उससे ऊपर उठकर मानव-प्रकृति के ऊध्र्वमुखीन विकास के साधन की अवस्था है; परम आत्मज्ञान, शक्ति और आनन्द की ओर मनुष्य के क्रमिक आरोहण की यह राजसिक अवस्था है। परन्तु यदि हम सदा इसी भूमिका पर ही बने रहें, जिसे गीता ने मध्यमा गतिः कहा है, तो हमारा आरोहण अधूरा ही रहता है, आत्मा का विकास अपूर्ण ही रहता है। जीव की सिद्धि का मार्ग सात्त्विक सत्ता और स्वभाव के भीतर से होकर उस पर पहुँचता है जो त्रिगुणातीत है।
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।। १९।।
१९. जब द्रष्टा यह देखता है कि गुण ही कर्ता हैं और कोई नहीं, और उस परम तत्त्व को जानता है जो गुणों से परे है, वह मेरे भगवद्भाव को प्राप्त हो जाता है।
जो भ्रान्ति प्रकृति के गुणों की क्रिया को स्वीकृति देती है उसे समाप्त होना होगा; क्योंकि जब तक इसे स्वीकार किया जाता है, तब तक आत्मा इनकी क्रियाओं में आबद्ध और इनके नियम के अधीन ही होती है।... गीता इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आत्म-साधना की एक नयी विधि बतलाती है। वह है गुणों की क्रिया से पीछे हटकर अपने अन्दर स्थित होना तथा प्रकृति की शक्तियों की तरंग के ऊपर विराजमान साक्षी की भाँति इस अस्थिर प्रवाह का निरीक्षण करना। साक्षी वह है जो देखता तो है पर तटस्थ एवं उदासीन बना रहता है, गुणों के निज स्तर पर उनसे पृथक् तथा अपनी सहज स्थिति में उनसे ऊपर उच्चासीन होता है। जब वे अपनी तरंगों के रूप में उठते-गिरते हैं, तब साक्षी उनकी गतिविधि देखता है, इसका निरीक्षण करता है, परन्तु न तो वह इसे स्वीकार करता है न इसमें क्षण भर भी हस्तक्षेप करता है। सबसे पहले निर्वैयक्तिक साक्षी की स्वतन्त्रता प्राप्त होना आवश्यक है: तदनन्तर स्वामी या ईश्वर का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है।
अनासक्ति की इस प्रक्रिया का प्रारम्भिक लाभ यह होता है कि व्यक्ति अपनी निज प्रकृति तथा समस्त विश्वप्रकृति को समझने लगता है। अनासक्त साक्षी अहंकार से लेशमात्र भी अन्धा हुए बिना प्रकृति की अविद्यामय शैलियों की क्रीड़ा को पूर्ण रूप से देख सकता है तथा उसकी सभी जटिलताओं, आच्छादनों एवं सूक्ष्मताओं में उसका पीछा करने अथवा उसे ढूँढ़ निकालने में समर्थ होता है क्योंकि यह छलरूप तथा छदावेश और जालबन्दी, - धोखेबाजी तथा छल-चातुरी से भरी हुई है। दीर्घ अनुभव से सीखा हुआ, सभी कार्यों एवं अवस्थाओं को गुणों की परस्पर क्रिया समझता हुआ, इनकी कार्यशैलियों से भिज्ञ होता हुआ वह और अधिक इनके आक्रमणों से परास्त नहीं हो सकता, इनके फन्दों में एकाएक फँस नही सकता अथवा इनके स्वांगों के धोखे में नहीं आ सकता। साथ ही वह देखता है कि अहं यथार्थ में इनकी परस्पर-क्रियाओं का साधन और इनकी थामे रखने वाली धारक ग्रंथि है और, यह जानकर, वह निम्न अहंकारमय प्रकृति की माया से मुक्त हो जाता है। वह परोपकारी और मुनि एवं मनीषी के सात्त्विक अहंकार से छूट जाता है, वह स्वार्थसेवी के राजसिक अहंकार को भी उस नियंत्रण से च्युत कर देता है जो उसने उसके प्राणिक-आवेगों पर जमा रखा है और अब वह निज स्वार्थ का परिश्रमी सेवक या पोषक तथा आवेश एवं कामना का सिरचढ़ा कैदी या अतिश्रम करनेवाला दंडित दास नहीं रहता; अज्ञानमय या निष्क्रिय, जड़ एवं बुद्धिहीन, तथा मानवजीवन के साधारण चक्र में फँसी हुई सत्ता के तामसिक अहंकार को वह अपनी ज्ञान-ज्योति से छिन्न-भिन्न कर देता है। इस प्रकार हमारे सभी व्यक्तिगत कर्म में अहंभाव-रूपी मूल दोष के विषय में निश्चित और सचेतन होकर वह अब और अधिक राजसिक या सात्त्विक अहंकार में आत्म-सुधार या आत्म-उद्धार का उपाय ढूँढ़ने की चेष्टा नहीं करता अपितु इनसे ऊपर एवं प्रकृति के उपकरणों तथा कार्यप्रणाली से परे केवल सर्वकर्म-महेश्वर तथा उसकी परम शक्ति या परा प्रकृति की ओर ही उन्मुख होता है। केवल वहीं समस्त सत्ता शुद्ध और मुक्त है और वहीं दिव्य सत्य का शासन सम्भव है।
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तो ऽमृतमश्नुते ।। २० ।।
२०. जब देहधारी जीवात्मा देह में उद्भूत होनेवाले इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और दुःखों से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व का आस्वादन करता है।
अर्जुन उवाच
कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।
किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ।। २१।।
२१. अर्जुन ने कहाः हे प्रभो! इन तीन गुणों से ऊपर उठा हुआ मनुष्य कित लक्षणों से युक्त होता है? वह किस प्रकार आचरण करता है और उसका व्यवहार किस प्रकार का होता है और किस साधन से वह इन तीन गुणों से परे जाता है?
श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ।। २२।।
२२. श्रीभगवान् ने कहाः हे पाण्डवा जो (सत्त्व जनित) प्रकाश से, (रजोजनित) कर्म में प्रवृत्ति से तथा (तमोजनित) मोह की वृद्धि से न तो द्वेष करता है और न ही उनके न रहने पर उनकी कामना करता है;
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ।। २३ ।।
२३. जो गुणों के प्रति उदासीन के समान और उनसे अविचलित बना रहता है, जो ऐसा जानकर कि केवल गुण ही क्रिया करते हैं उनसे तटस्थ, अचल बना रहता है।
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिंदात्मसंस्तुतिः ।। २४।।
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।। २५।।
२४-२५. जो आत्मस्थ और अविचलित मनुष्य दुःख और सुख में समान रहता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है, प्रिय और अप्रिय को समान समझता है, अपनी निन्दा और प्रशंसा में समान रहता है, मान और अपमान में समान रहता है, जिसके लिए मित्रदल और शत्रुदल एक समान हैं, और जिसने कार्यों के आरंभ की समस्त प्रवृत्ति को त्याग दिया है, वह गुणातीत कहा जाता है।
[तीनों गुणों से अनासक्त श्रेष्ठता की स्थिति में] आत्मा निम्न प्रकृति से आन्तरिक रूप से पृथक् तथा स्वतन्त्र होती है, इसकी कुण्डलियों में फंसी हुई नहीं होती, इसके ऊपर उदासीन और प्रसन्न भाव में स्थित रहती है। प्रकृति अपने पुराने अभ्यासों के त्रिविध चक्र में कार्य करती रहती है, - कामना, हर्ष और शोक हृदय को आक्रांत करते हैं, सभी साधन-उपकरण अकर्मण्यता, जड़ता एवं खिन्नता के गर्त में जा गिरते हैं, प्रकाश और शान्ति हृदय, मन तथा शरीर में फिर लौट आते हैं; किन्तु आत्मा इन परिवर्तनों से अपरिवर्तित और अप्रभावित बनी रहती है। निम्न अंगों की वेदना तथा कामना का निरीक्षण करती हुई पर उनसे अचलायमान, उनके हर्षों और प्रयासों पर मुस्कराती हुई, विचार की भ्रान्तियों तथा धूमिलताओं को और हृदय तथा स्नायुओं की उच्छृंखलता एवं दुर्बलताओं को समझती हुई पर उनसे पराभूत न होती हुई, प्रकाश एवं प्रसन्नता के लौटने पर मन के अन्दर उत्पन्न ज्ञान-आलोक तथा सुख-आराम से और उसके विश्राम एवं बल-सामर्थ्य के अनुभव से मोहित तथा इसमें आसक्त न होती हुई आत्मा अपने को इनमें से किसी भी चीज में झोंकती नहीं, किन्तु अविचलित रहकर उच्चतर इच्छाशक्ति के निर्देशों तथा महत्तर एवं प्रकाशपूर्ण ज्ञान की स्फुरणाओं की प्रतीक्षा करती है।
यह ब्राह्मी स्थिति की निर्व्यक्तिकता है... परन्तु फिर भी यहाँ स्पष्ट रूप से एक द्वैत स्थिति है, सत्ता दो विपरीत भागों में अक्षर और क्षर में खंडित है, अक्षर पुरुष या ब्रह्म में मुक्त हुई आत्मा अमुक्त क्षर प्रकृति की क्रिया का निरीक्षण करती है। क्या कोई इससे महान् स्थिति नहीं है, पूर्णतर पूर्णता का कोई तत्त्व नहीं है, अथवा क्या यह विभाजन ही देह में प्राप्य उच्चतम चेतना है, और क्या इस क्षर प्रकृति का तथा प्रकृति के अन्दर देह-धारण से उत्पन्न गुणों का त्याग और ब्रह्म की निर्व्यक्तिकता तथा नित्य शांति में लय ही योग का लक्ष्य है? क्या व्यष्टि-पुरुष का यह लय ही परम मोक्ष है? ऐसा प्रतीत होता है कि कोई और वस्तु भी है; क्योंकि बार-बार अपने निर्णायक स्वर पर लौटते हुए, गीता इसे उपसंहार के रूप में कहती है...
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। २६।।
२६. और जो अविचल (अव्यभिचारी) भक्तियोग के साथ मुझसे प्रेम करता है और मेरी उपासना करता है, वह इन गुणों से परे पहुँच जाता है और बहा होने के लिये तैयार हो जाता है।
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७॥
२७. मैं ही ब्रह्म का, अमृतत्व और अविनाशी सत्ता का तथा सनातन धर्म का और परम-आनंदरूप सुख का आधार हूँ।
अद्वैतवादियों का यह कहना है कि इस पार्थिव अभिव्यक्ति में कोई भी तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ सकता। शंकराचार्य आदि का कहना है कि जब स्वयं परमात्मा भी अवतार ग्रहण कर के इस धरती पर आते हैं तब उन पर भी तीनों गुण लागू होते हैं और उनकी क्रिया त्रिगुणमयी होती है। इसलिए संसार में कर्म करना मूर्खता है। श्रीअरविन्द गीता के विवेचन में कहते हैं कि गीता सूक्ष्म रूप से इसका प्रतिपादन करती है कि इस देह में रहते हुए भी तीनों गुणों से ऊपर उठा जा सकता है और उस स्थिति में कर्म किया जा सकता है। हमारे ऋषि-मुनि कहते हैं कि भगवान् तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं। परंतु जब हम उनकी लीला-कथाएँ पढ़ते हैं तब उनमें तो हमें भगवान् की क्रियाएँ भी गुणों से प्रभावित प्रतीत होती हैं। इसी को देखकर अद्वैतवादी कहते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर तो व्यक्ति केवल अक्षर ब्रह्म में जाने पर ही हो सकता है अन्यथा नहीं। परंतु अद्वैतवादी जिस अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं उस स्थिति में तो केवल हमारा पुरुष पक्ष ही अवस्थित हो सकता है, बाह्य प्रकृति नहीं। पुरुष के अक्षर की शांति में स्थित होने पर भी प्रकृति में तो सुख-दुःख, शीत-उष्ण आदि द्वंद्व तथा अन्य त्रिगुणमय विकार तो चलते ही रहेंगे। अतः पुरुष तो त्रिगुणों से परे चला जाता है परंतु प्रकृति त्रिगुणमय प्रपंच में फंसी रहती है। इसीलिए कर्म करते ही तो व्यक्ति त्रिगुणों में फँस जाता है। श्रीअरविन्द का कहना है कि गीता के अनुसार प्रकृति के अंदर भी तीनों गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। यही विशेष बात है। परंतु बिना इसका अनुभव हुए यह बात समझ में नहीं आ सकती।
वास्तव में चेतना का एक ऐसा स्तर है जहाँ व्यक्ति को प्रत्येक चीज में आनंद आने लगता है। जिसे बाहरी रूप से सुख कहते हैं वह भी उसके लिए उतना ही आनंददायी होता है जितना कि वह जिसे दुःख कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे किसी प्रिय व्यक्ति के लिए हमें कष्ट उठाना पड़े तो हमें उसमें कष्ट का अनुभव न होकर गहरे सुख का अनुभव होता है कि हम उस प्रिय व्यक्ति के कुछ काम आ सके। वहीं जिसे इस प्रेम भाव का अनुभव न हो उसे तो सारी क्रिया कष्टमय प्रतीत होगी। अतः केवल चेतना के परिवर्तन से ही हम देख सकते हैं कि समान ही स्थिति में एक व्यक्ति को परम् आनंद की अनुभूति हो सकती है और दूसरे को उसमें कष्ट का अनुभव हो सकता है। इसी प्रकार एक ऐसी चेतना है जिसमें स्थित होने पर व्यक्ति पर त्रिगुण बाध्यकारी नहीं रहते, हालाँकि बाहरी रूप से दूसरों को उसकी क्रियाएँ त्रिगुणमय प्रतीत हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी नाटक में कोई भाग अदा कर रहा है जिसमें उसे दुःख-कट, यंत्रणा, वियोग आदि की भूमिका निभानी होती है तो भले वह अपनी भूमिका को इतनी भली-भाँति निभाता है कि दर्शकगण भी स्तब्ध और रोमांचित हो जाते हैं परंतु उस पात्र को तो पता होता है कि वह केवल नाटक कर रहा है और ऐसे में वह बाहरी रूप से जो भी भाव क्यों न अभिव्यक्त कर रहा हो परंतु भीतर से उस सब से अप्रभावित बना रहता है। इसलिए भगवान् के प्रति भक्ति आने पर जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है तब उसे इस दृश्य जगत् का रहस्य पता चल जाता है। तब वह चेतना के एक ऐसे स्तर पर निवास करने लगता है जहाँ वह बाहरी चीजों में आसक्त नहीं रहता और इसी कारण सच्चे रूप से वह गुणों से अप्रभावित रहते हुए भी अपनी क्रिया भली-भाँति कर सकता है। यही पुरुषोत्तम भाव का रहस्य है। वह उतने ही सफल रूप से क्षर भाव अपनाकर अपनी क्रिया कर सकता है जितना कि अक्षर भाव अपनाकर और फिर भी वह इन दोनों ही भावों से परे रहता है और इसीलिए वह बिना गुणों में बँधे मुक्त रूप से अपनी क्रिया कर सकता है। अब यदि व्यक्ति को यह पता हो कि नाटक के अंदर उसे खलनायक की भूमिका निभानी है और उसमें उसे नायक के हाथों हार, अपमान आदि सहना है तो ऐसा करने में भी वह अपनी भूमिका अच्छे से अच्छे ढंग से निभाने का प्रयास करेगा और इसमें भीतर से उसके किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उल्टे, जितने ही अच्छे ढंग से वह अपनी भूमिका निभाता है उतना ही वह आत्म-संतुष्ट होता है भले ही नाटकीय प्रतीति जो भी हो। अतः जब व्यक्ति एक ऐसी चेतना में स्थित होता है जहाँ उसे भगवान् की अभिव्यक्ति का, उनकी लीला का, उनकी अधिकाधिक गहराइयों के उन्मीलन का रहस्य, विधान तथा औचित्य कुछ-कुछ समझ में आने लगता है तब भले बाहर से प्रतीति कुछ भी क्यों न हो, परंतु वस्तुतः वह तो सभी द्वंद्वों को समान ही भाव से लेता है क्योंकि तब उसे किसी भी चीज के प्रति किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रहती, उल्टे चीजों के रहस्य को जानकर वह हर चीज में आनंद लेने लगता है। अब यदि अपने प्रेमास्पद के लिए कोई मिठाई तैयार कर रहा हो और उस प्रक्रिया में बहुत श्रम लगता हो, तेज गर्मी सहन करनी पड़ती हो, तो भी वह प्रेमभाव सारी क्रिया के श्रम को हर लेता है और उसे आनंद में परिणत कर देता है। अतः जब सारे संसार में व्यक्ति अपने दिव्य प्रेमास्पद को देखता है तो उनके लिए कार्य करने में उसके लिए कहीं गुणों की कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। उसे तो हर चीज में ही आनंद आने लगता है क्योंकि उसकी सभी क्रियाएँ अपने प्रेमास्पद के निमित्त प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाती हैं। अतः भगवान् के साथ प्रेम ही वह आधार है जो सभी गुणों से परे ले जाता है और सभी कुछ को आनंद में परिणत कर देता है। प्रेम ज्ञान की पराकाष्ठा है क्योंकि जब अपने प्रेमास्पद के स्वरूप का ज्ञान होता है तब प्रेम स्वतः ही आ जाता है और ज्यों ही प्रेम होता है त्यों ही व्यक्ति अपने प्रेमास्पद की और अधिक गहराइयों में पैठता जाता है। और जब व्यक्ति अधिकाधिक उन गहराईयों में रमण करता है और जीवन में उन्हीं को अभिव्यक्त करता है तब इसमें गुणों की कोई बाध्यता नहीं रहती। उस चेतना में गुणों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। यह स्थिति मनुष्य शरीर में भी संभव है। और यह स्थिति समता या उदासीनता की स्थिति नहीं है जिसमें कि व्यक्ति किसी भी चीज में लिप्स नहीं होता अपितु यह तो आनंद की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने प्रेमास्पद के लिए बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया या संकोच के घोर से घोर कर्म करने में भी संकोच नहीं करता है क्योंकि उसकी चेतना के लिए उसे वह कर्म घोर प्रतीत नहीं होता अपितु उसे तो उसमें भी आनंद की अनुभूति होती है। परंतु बाहरी रूप से दूसरा कोई भी यह नहीं जान सकता कि उस व्यक्ति की क्रिया त्रिगुणों के प्रभाव से ऊपर है क्योंकि बाहरी रूप से तो वे कर्म त्रिगुणमय प्रतीत हो सकते हैं।
अतः करने का कार्य यह है कि किसी भी प्रकार हमारा मन भगवान् के किसी रूप में लग जाए, साथ ही, यदि किसी को सशरीर विद्यमान गुरु की सेवा करने का परम् सौभाग्य प्राप्त हो तो इससे श्रेष्ठ तो कोई बात हो ही नहीं सकती। परंतु इसमें यह समझना होगा कि जब व्यक्ति के अंदर भगवान् के प्रति भक्ति आती है और वह पुरुषोत्तम भाव की ओर अग्रसर हो रहा होता है तब संभवतः कुछ चीजों में तो वह आनंद ले पाता है परंतु उसकी सत्ता में कुछ ऐसे भाग भी हैं जो उस आनंद में अभी सहभागी नहीं हो पाते और अपने ही निम्नतर हेतुओं की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। अतः ज्यों-ज्यों व्यक्ति अधिकाधिक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है त्यों-त्यों अन्य भाग भी भगवान् में आनंद लेने लगते हैं। हालाँकि जड़भौतिक और निश्चेतन स्तरों की गुत्थी तो बिना अतिमानसिक रूपांतर के सुलझाई नहीं जा सकती, परंतु फिर भी गुणों से परे की क्रिया तो भौतिक रूपांतर से पहले भी संभव है। क्योंकि गीता भौतिक रूपांतर तक नहीं जाती। इसलिए यदि गीता इस त्रिगुणों से परे की स्थिति का वर्णन करती है तो इसका अर्थ है कि भौतिक रूपांतर होने से पूर्व भी त्रिगुणातीत अवस्था संभव है। भगवान् की भक्ति के द्वारा यह स्थिति संभव है। इस अध्याय के अंतिम दो श्लोकों में भगवान् पहले कहते हैं कि "जो अविचल (अव्यभिचारी) भक्तियोग के साथ मुझसे प्रेम करता है और मेरी उपासना करता है, वह इन गुणों से परे पहुँच जाता है और ब्रह्म होने के लिये तैयार हो जाता है।" परंतु ब्रह्म का आधार भी तो स्वयं भगवान् ही हैं। इसीलिए अगले ही श्लोक में भगवान् कहते हैं "मैं ही ब्रह्म का, अमृतत्व और अविनाशी सत्ता का तथा सनातन धर्म का और परम-आनंदरूप सुख का आधार हूँ।"
इस प्रकार चौदहवाँ अध्याय 'गुणत्रयविभागयोग' समाप्त होता है।
पन्द्रहवाँ अध्याय
तीन पुरुष
गीता की शिक्षा, शुरू से अंत तक, अपनी सभी धाराओं में तथा अपने समस्त नमनीय मोड़ों के द्वारा एक ही केंद्रीय विचार की ओर मुड़ती है, और उस विचार तक यह विभिन्न दार्शनिक पद्धतियों के मतभेदों का हर तरह से अपना संतुलन और सामंजस्य साधित करती हुई तथा आध्यात्मिक अनुभूति के सत्यों का अपना सावधानीपूर्वक समन्वय साधित करती हुई अग्रसर होती है। उन सत्यों अथवा प्रकाशों को यदि पृथक् पृथक् लिया जाए तथा उनके आलोक की बाह्य रश्मियों एवं कलाओं का एकांगी रूप से अनुसरण किया जाए तो वे प्रायः परस्पर विरोधी या, कम-से-कम, भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ उन सबको एकत्र कर समन्वयकारी दृष्टि के एक ही केंद्र में गूँथ दिया गया है। यह केंद्रीय विचार त्रिविध चेतना का विचार है जो तीन होती हुई भी एक है तथा सत्ता की संपूर्ण श्रृंखला में विद्यमान है।
जो पुरुष प्रकृति की क्रिया को, उसके परिवर्तनों को, उसके क्रमागत भूतभावों को सीधा अनुप्राणित करता है वह क्षर पुरुष है, जो प्रकृति के परिवर्तनों के साथ परिवर्तित होता, प्रकृति की गति के साथ चलता प्रतीत होता है, वह व्यष्टि पुरुष है जो प्रकृति के सतत् कर्म-प्रवाह से अपने व्यक्तित्व में होनेवाले परिवर्तनों के साथ तदाकार हुआ चलता है।.... प्रकृति में व्यक्त और उसके कर्म में बद्ध पुरुष के परे पुरुष की एक और स्थिति भी है, जो केवल एक स्थितिशील अवस्था है, वहाँ कर्म बिल्कुल नहीं है; वह पुरुष की नीरव-निश्चल, सर्वगत, स्वतःस्थित, अचल, अक्षर आत्मसत्ता है, भूतभाव नहीं।. .... मनुष्य का आत्मा (पुरुष) जब क्षरभाव अपनाता है तब अपने-आप को व्यक्तित्व के खेल के साथ तदात्म कर लेता है और प्रकृतिगत अहंभाव से अपने आत्म-ज्ञान को इच्छापूर्वक आच्छादित कर लेता है और इस तरह अपने-आप को कर्मों का कर्ता समझने लगता है; और जब यह आत्मा (पुरुष) अक्षर भाव में आता है तब अपने-आप को नैयक्तिक भाव के साथ एक कर लेता है और उसे यह बोध होता है कि कर्ती प्रकृति है, वह स्वयं तो निष्क्रिय साक्षी पुरुष है, अकर्तारम्। मनुष्य के मन को दो भावों में से किसी एक भाव की ओर झुकना पड़ता है, मन इन दो भावों को दो भिन्न विकल्पों के रूप में लेता है; या तो वह गुण और व्यक्तित्व के क्षरभावमय कर्म में जाकर प्रकृति के द्वारा बँध जाता है, या फिर अक्षर नैव्यक्तित्व में जाकर प्रकृति की क्रियाओं से मुक्त हो जाता है।
परन्तु यथार्थ में पुरुष की निज-स्थिति और अक्षरभाव तथा प्रकृति में कर्म और क्षरत्व, दोनों एक साथ ही रहते हैं। यह एक ऐसी असमाधेय विसंगत कर्म और भजसके समाधान के लिए या तो मायावाद जैसे किसी वाद का आश्रय लेना पड़ता या आत्मा को दोहरी और विभक्त सत्ता वाला मानना पड़त्ता यदि आत्मा की सत्ता का ऐसा परम भाव न होता जिसके ये दोनों विपरीत पहलू हैं, और जो स्वयं इनमें से किसी से सीमित नहीं है। हमने देखा है कि गीता इस परम भाव को पुरुषोत्तम के भाव में पाती है।
मायावादी लोग पुरुषोत्तम भाव को स्वीकार नहीं करते इस कारण केवल क्षर और अक्षर दो भेद रह जाते हैं। अब चूंकि क्षर और अक्षर दोनों एक दूसरे से विपरीत भाव हैं इसलिए मायावादी जगत् को मिथ्या बताकर अक्षर ब्रह्म का चयन करते हैं और उसी में स्थित होने पर बल देते हैं। मायावाद के अनुसार यदि व्यक्ति कर्म में लिप्त है तो वह अज्ञानी है। इसलिये उसे चाहिये कि वह कर्म का त्याग कर अक्षर पुरुष से तदाकार हो जाये। परंतु यदि गीता भी इसी का प्रतिपादन करती तब तो अर्जुन को युद्ध का आदेश देना एक सर्वथा विसंगत बात होती जबकि अर्जुन तो स्वयं ही युद्ध से विरत होने के लिए तत्पर था। इसलिए उनके अनुसार श्रीकृष्ण को भी आध्यात्मिक व्यक्ति के स्थान पर कर्मवादी और भोगवादी व्यक्ति ही मानना चाहिये जो कि अर्जुन को युद्ध करने और उसमें विजय के पश्चात् राज्य के भोग के लिये प्रेरित कर रहे हैं।
यदि जीव का, जैसा कि मायावाद का मत है, किसी भी प्रकार अक्षर ब्रह्म में स्थित होकर समस्त कर्मों का त्याग कर देना और इस जगत् प्रपंच से अपने को विलग कर लेना ही एकमात्र उद्देश्य होता तब तो इसका कोई कारण समझ नहीं आता कि परमात्मा की ऐसी क्या बाध्यता होगी कि वे ऐसे संसार का सृजन करें जिसमें से छूट निकलना ही एकमात्र उद्देश्य हो। ये सारे प्रश्न मानसिक स्तर पर नहीं सुलझाये जा सकते। एक समय जब स्वयं श्रीअरविन्द इसी प्रश्न पर चिंतनरत थे तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अंतर्दर्शन में कहा कि मन के स्तर पर देखने पर ही हमें जगत् के विषय में वैसा निरुद्देश्य दृष्टिकोण प्राप्त होता है। सच्चा दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए सचेतन रूप से मन से उच्चतर स्तरों पर आरोहण करना होगा तभी इस सारी अभिव्यक्ति का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है।
इसे समझने के लिए हम इस संसार को एक नाटक के समान मान सकते हैं जिसको परमात्मा ने अपनी प्रसन्नता के लिये रचा है। इसमें भूमिका निभाने वाले अलग-अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं। पहला कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि अपनी भूमिका से ही तदाकार हो जाये और यह भूल जाये कि वह तो नाटक का ही हिस्सा है और अपनी भूमिका से सुखी अथवा दुःखी होता रहे। यह क्षर भाव है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो कि अपनी भूमिका से परेशान होकर नाटक से अलग होकर ही बैठ जाये। यह अक्षर भाव है। तीसरा एक व्यक्ति ऐसा है जो कि नाटक के रचयिता से तदाकार है और नाटक का उद्देश्य भली-भाँति जानता है और अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाता है और नाटक की सफलता के लिये स्वयं को समर्पित कर देता है। यह पुरुषोत्तम भाव है। और वास्तव में तो किसी कलाकार का नाटक से अलग होकर बैठ जाना भी नाटक का ही भाग है। यह भी एक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।
पुरुषोत्तम संबंधी विचार को शुरू से ही तैयार किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है, इसका पूर्वाभास दिया जा चुका है, इसे अपनाया गया है, परंतु केवल अब जाकर पन्द्रहवें अध्याय में ही इसे स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है और अब ही इसे एक नाम देकर पुरुषत्रय के भेद पर प्रकाश डाला गया है। और यह देखना बोधप्रद होगा कि कैसे तुरंत ही इस विषय में प्रवेश करके इसका विकास किया जाता है। हमें बताया जा चुका है कि दिव्य प्रकृति में आरोहण करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने-आप को पूर्ण आध्यात्मिक समता में प्रतिष्ठित करना होगा तथा त्रिगुणात्मिका निम्नतर प्रकृति से ऊपर उठना होगा। इस प्रकार निम्नतर प्रकृति को पार कर हम अपने-आप को सुप्रतिष्ठित कर लेते हैं निर्व्यक्तिकता में, समस्त कर्म से अविचल श्रेष्ठ स्थिति में, त्रिगुण जनित समस्त परिसीमन और परिबंधन से विशुद्ध स्थिति में, और यह स्थिति पुरुषोत्तम की व्यक्त प्रकृति का एक पक्ष है, आत्मा की शाश्वतता तथा एकता, अक्षर, के रूप में उनकी अभिव्यक्ति है। परन्तु जीव की अभिव्यक्ति के आदि रहस्य के पीछे पुरुषोत्तम का एक अनिर्वचनीय शाश्वत अनेकत्व, एक परमोच्च सत्यतम सत्य भी है। अनंत भगवान् की एक सनातन शक्ति है, उनकी दिव्य प्रकृति की एक अनादि और अनन्त क्रिया है और उस क्रिया में निर्व्यक्तिक दिखनेवाली शक्तियों की क्रीड़ा मैं से जीव-रूपी आश्चर्य प्रकट होता है, प्रकृतिर्जीवभूता। इस आश्चर्य के संभव होने का कारण यह है कि व्यक्तित्व भी भगवान् का ही एक रूप है और वह अनंत में अपना सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य एवं सार्थकता प्राप्त करता है। परन्तु अनंत के भीतर स्थित 'पुरुष' निम्नतर प्रकृति का अहंपरक, भेदमूलक, विस्मृतिपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है; वह तो एक उदात्त, विश्वमय और विश्वातीत, अमर और दिव्य सत्ता है। उन परम् पुरुष का यह रहस्य ही प्रेम और भक्ति का गुप्त मर्म है। हमारा अंतरस्थ आध्यात्मिक पुरुष, नित्य जीवात्मा अपने-आप को तथा उसके पास जो कुछ भी है और वह स्वयं जो कुछ है उस सबको उन शाश्वत भगवान्, परम् पुरुष एवं परमेश्वर के प्रति अर्पित कर देता है जिनका कि वह एक अंश है। इस आत्मदान में ही, अपने व्यक्तित्व तथा इसके कमौ के अनिर्वचनीय प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति के द्वारा अपनी वैयक्तिक प्रकृति को इस प्रकार ऊपर उठा ले जाने में ही ज्ञान अपनी पूर्णता लाभ करता है: कर्मों का यज्ञ इसके द्वारा अपनी सिद्धि और पूर्ण स्वीकृति या प्रामाणिकता प्राप्त करता है। अतः, इन चीजों के द्वारा ही मनुष्य की आत्मा इस अन्य शक्तिशाली क्रियाशील रहस्य में, दिव्य प्रकृति के इस अन्य महान् एवं अंतरीय अंग में अपनी पूर्णतम चरितार्थता प्राप्त करती है और उस पूर्णता के द्वारा अमृतत्व, परम सुख एवं शाश्वत धर्म का आधार उपलब्ध करती है। और, इस प्रकार गीता ने पहले तो एकमेव आत्मा में समता तथा एकमेव परमेश्वर को आराधना इन दो आवश्यक साधनों का पृथक् पृथक् प्रतिपादन किया है मानो ये ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के, 'ब्रह्मभूयाय', दो भिन्न-भिन्न साधन हों, - एक तो निवृत्तिमार्गी संन्यास का मार्ग हो और दूसरा दिव्य प्रेम एवं दिव्य कर्म का। परन्तु इसका प्रतिपादन करने के बाद अब गीता वैयक्तिक और निर्व्यक्तिक को पुरुषोत्तम में एकीभूत करने तथा उनके संबंधों का निरूपण करने की ओर अग्रसर होती है। क्योंकि गीता का लक्ष्य एकांगी भावों तथा भेदकारी अतिरंजनाओं से मुक्त होना तथा ज्ञान एवं आध्यात्मिक अनुभव के इन दो पक्षों को घुला-मिला कर परम सिद्धि के एक ही पूर्ण पथ में परिणत कर देना है।
यहाँ सबसे पहले गीता अश्वत्थ वृक्ष के वेदांतिक रूपक की भाषा में जगत् का वर्णन करती है।
श्रीभगवान् उवाच
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ।। १।।
१. श्रीभगवान् ने कहाः जिसकी जड़ें ऊपर की ओर, जिसकी शाखाएँ नीचे की ओर हैं, ऐसे अश्वत्थ (पीपल के पेड़) को अनश्वर कहा जाता है, जिसके पत्ते (वेदों के) मंत्र हैं, और जो इसे जानता है वह वेद का ज्ञाता' है।
अधश्वोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
अधश्व मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥
२. गुणों द्वारा पोषित इस वृक्ष की शाखाएँ नीचे और ऊपर दोनों ओर फैली हुई हैं; इन्द्रियों के विषय उसके पत्ते हैं; और नीचे की ओर मानवलोक में इसकी जड़ें फैली हुई हैं जो मनुष्यों को कर्म से बाँधती हैं।
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।। ३।।
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । त
मेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ।। ४।।
३-४. जैसा वर्णन किया गया है हमें यहाँ इसका वास्तविक रूप वैसा दिखायी नहीं देता, न इसका अन्त और न आदि और न आधार ही दिखायी देता है। इस दृढ़मूल अश्वत्थ को अनासक्ति की बलशाली तलवार से काटकर व्यक्ति को उस पद (परम लक्ष्य) का - जिस पर पहुँचने पर फिर पुनः लौटना नहीं होता - अन्वेषण यह कह कर करना चाहिये कि "मैं एकमात्र उन आदि पुरुष की शरण ग्रहण करता हूँ जिनसे कर्म की ओर शाश्वत प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।"
अश्वत्थ वृक्ष का जो रूपक दिया गया है उसे हम इस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि यह भगवान् की अभिव्यक्ति का रूपक है। यह अभिव्यक्ति अनादि और अनंत है और इसका कोई ओर-छोर नहीं है। यह तो शाश्वत है। इसके स्रोत के विषय में भी हम नहीं जानते। इस अभिव्यक्ति में निम्न वृत्तियाँ भी हैं जिनकी गति नीचे की ओर होती है और ऊर्ध्वमुखो वृत्तियाँ भी हैं। और यह अभिव्यक्ति केवल अतिचेतन स्तरों तक ही सीमित नहीं है अपितु यह अवचेतन और निश्चेतन स्तरों तक भी फैली हुई है। पेड़ के ऊपर से जो जड़े चलती हैं उन्हें हम अपनी प्राणिक वृत्तियों के रूप में मान सकते हैं जो कि हमें जड़तत्त्व से बाँध देती हैं। परंतु यह सारी अभिव्यक्ति हमें त्रिगुणमयी प्रतीत होती है। हमारे वेद संपूर्ण अभिव्यक्ति की पूरी संरचना का वर्णन करते हैं। हमारी इंद्रियाँ हमें इस पूरी संरचना के विषय में बोध कराती हैं और ज्यों-ज्यों चेतना का विकास होता जाता है त्यों-त्यों वे ही इंद्रियाँ हमें अभिव्यक्ति के अधिक गहरे रहस्यों को गोचर करवाने लगती हैं।
_______________
*.वेद या कम-से-कम वेदवाद के संबंध में जो किंचित् अपमानजनक विचार हम पहले देख आये हैं उसका आशय हमें यहाँ समझ में आ जाता है। क्योकि जो ज्ञान वेद हमें प्रदान करता है वह देवताओं, सृष्टि के मूल तत्त्वों एवं शक्तियों का ज्ञान है, और इसके फल कामनापूर्वक किये जानेवाले यज्ञ के फल हैं, तीन लोकों की, भूलोक, द्युलोक तथा अंतरिक्षलोक की प्रकृति में उपभोग एवं प्रभुत्वरूपी फल हैं।... वेद के छंद, छंदांसि, पते हैं तथा सब इंद्रियभोग्य विषय, जो यथाविधि यज्ञ करने से सर्वोत्तम रूप में प्राप्त होते हैं, निरंतर प्रस्फुटित होनेवाले पल्लव हैं।
यहाँ तक कि अतिमानसिक स्तर की अपनी इंद्रियाँ होती हैं जो सत्य का बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन कराती हैं। तो यह सारा रूपक इस पूरी अभिव्यक्ति का है। भारतीय परंपरा में सदा ही ऐसा प्रचलित रहा है कि व्यक्ति जब तक इस अभिव्यक्ति से अभिभूत रहता है, इसमें आसक्त रहता है तब तक वह शाश्वत की ओर नहीं जा सकता। इसलिए इससे निकलने का रास्ता वेदों ने यज्ञ के आरोहण के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें व्यक्ति अपनी जिस किसी वर्तमान स्थिति से आरंभ कर अपने सच्चे स्वरूप की ओर आरोहण कर सकता था। साथ ही कालांतर में मायावादी दृष्टिकोण आने के बाद इस प्रपंच से छूट निकलने का मार्ग भी प्रचलित रहा है। इस दृष्टिकोण में तो वेदों को भी त्रिगुणमय ही बताया गया है। इसी प्रचलित भाव को दूसरे अध्याय के पैंतालीसवें श्लोक में गीता प्रतिध्वनित करते हुए कहती है 'त्रैगुण्यविषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन'। इसी को आधार मानकर लोग कहते हैं कि स्वयं गीता वेदों को त्रिगुणमय बताकर अवमानित करती है। परंतु गीता में ही भगवान् वेदों का प्रतिपादन भी करते हैं और विभूतियोग में कहते हैं कि वेदों में वे सामवेद हैं और इस अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में भगवान् कहते हैं कि "मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य एकमेव हूँ। मैं ही वेदान्त का रचयिता और वेद का ज्ञाता हूँ।" अतः यह समझना चाहिये कि गीता वेदों का खण्डन नहीं करती अपितु किसी समय विशेष पर उत्पन्न हुई वेदवाद की रूढ़िवादिता का खण्डन करती है। यह खण्डन इसलिए आवश्यक था क्योंकि यज्ञ, तप आदि का तथा वेद मंत्रों का तामसिक, राजसिक और सात्विक हेतुओं और उपलब्धियों की पूर्ति लिए दुरुपयोग किया जाने लगा था। और इसलिए ये सभी क्रियाएँ केवल बंधन का कारण विनती थीं, इसीलिए यहाँ तलवार से काटने का उल्लेख आया है। हालाँकि गीता अपनी शिक्षा को इन बंधनों को काटने तक ही सीमित नहीं रखती अपितु वह तो सभी धर्मों का परित्याग कर अनन्य रूप से भगवान् के पास जाने को कहती है। जब एक बार व्यक्ति इन बंधनों को काटकर भगवान् पर आश्रित हो जाता है तभी सच्चे कर्म कर सकता है। यही बात इस श्लोक से झलकती है कि 'मैं एकमात्र उन आदि पुरुष की शरण ग्रहण करता हूँ जिनसे कर्म की ओर शाश्वत प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।' परंतु कर्मों की ओर प्रवृत्ति की बात कर के गीता ने अद्वैतवादियों के सारे समीकरण को ही बिगाड़ दिया। अब यदि व्यक्ति एक ही श्लोक में कर्मबंधन और कर्मप्रवृत्ति की बात देखता है तो उसे गीता में विरोधाभास प्रतीत होता है जबकि वास्तव में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। सच्चे कर्मों का आरंभ तो तभी हो सकता है जब उनका उत्प्रेरण शाश्वत सत्ता के द्वारा किया जाता है। और तब कर्म बंधनस्वरूप नहीं रह जाते अपितु आत्म-अभिव्यक्ति के साधन बन जाते हैं। वहीं यदि अहंमय रूप से किये जाएँ तब वे बंधन का कारण बन जाते हैं। यह एक सूक्ष्म भेद है जिसे समझने पर किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं रहता। शाश्वत द्वारा कर्मों का उत्प्रेरण कैसे होगा इस तत्त्व को गीता पुरुषोत्तम तत्त्व के निरूपण में बतलाएगी।
सर्वत्र ही हम गीता की यह विलक्षणता पाते हैं कि सभी सिद्धांतों, दर्शन-पद्धतियों आदि का सारतः निरूपण करने के बाद वह उन्हें अपने ही भाव में समन्वित कर लेती है जिसके कारण वे सभी चीजें अपना एकांगी स्वरूप छोड़कर व्यापक बन जाती हैं। त्रिगुणों का विस्तार से वर्णन करने के बाद उनसे ऊपर उठने को भी भक्ति तत्त्व के निरूपण के द्वारा गीता ने कोई नीरस विषय न छोड़कर एक आनंद का विषय बना दिया है। और वास्तव में तो किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सच्ची आंतरिक परिपूर्ति के बिना हो भी नहीं सकता क्योंकि पुरुषोत्तम का स्वरूप एकांगी और नीरस नहीं अपितु सर्वसमावेशी, सर्वालिंगनकारी और आनंदमय है। एकांगी तो अक्षर पुरुष है। अतः संकेत रूप में गीता ने यहाँ पुरुषोत्तम को कर्मों के स्रोत के रूप में बताया है।
प्रश्न : यहाँ सारी अभिव्यक्ति को अश्वत्थ का रूपक दिया गया है तो एक ओर तो इसे अनश्वर कहा गया है और दूसरी ओर उसे तलवार लेकर काट डालने की बात कही गई है, तो यह परस्पर विपरीत बात कैसे?
उत्तर : जितने भी मायावादी हैं वे इस संसार को नश्वर बताते हैं और केवल ब्रह्म को ही अनश्वर और सत्य बताते हैं। पर इसमें समझने की बात है कि संसार अपने आप में नष्ट नहीं होता, जिन मन, प्राण, शरीर रूपी माध्यमों से हम उसे देखते हैं वे नश्वर हैं। अपने आप में जो सृष्टि है वह शाश्वत है परंतु उसके अंदर अभिव्यक्त हुए जो घटक हैं वे अभिव्यक्ति में आते-जाते रहते हैं जिसे हम जन्म-मृत्यु कहते हैं। इसलिए यह जागतिक अभिव्यक्ति अपने आप में अविनश्वर है परंतु इसके पदार्थ नश्वर हैं जो अपने समय से आते हैं और अपना समय समाप्त होने के बाद पुनः अभिव्यक्ति से बाहर चले जाते हैं। अतः इसमें यह सूक्ष्म भेद निहित है। यदि व्यापक रूप से देखें तो सारी गोचर अभिव्यक्ति भगवान् के विविध पहलुओं की ही तो अभिव्यक्ति है और वह समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए इसे हम नश्वर कह सकते हैं और जो मूलतत्त्व जिससे सभी पहलू अभिव्यक्त होते हैं वह स्वयं अविनश्वर है। अतः इसका यह अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिये कि किसी समय सृष्टि नहीं थी और किसी समय विशेष पर वह आरंभ हुई। परंतु हमारे मन के लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि किस प्रकार सृष्टि शाश्वत है जिसका कि कोई आरंभ नहीं है। जब परम प्रभु आत्म-संवरण कर लेते हैं तब सृष्टि आदि सब उन्हीं में समाहित हो जाती है। उस स्थिति की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। परंतु तब भी सारी सृष्टि निहित तो परम प्रभु में ही रहती है। परंतु जब वे अपनी पराप्रकृति के द्वारा अपने पहलुओं को अभिव्यक्त करते हैं तब उसे हम सृष्टि कहते हैं। अतः इस अर्थ में सृष्टि तो सदा ही विद्यमान रहती है। यदि वह अभिव्यक्ति में न भी हो तो भी परम प्रभु में तो वह निहित होती ही है हालाँकि सामान्य तौर पर हम उसे सृष्टि नहीं कहेंगे क्योंकि वह गोचर अभिव्यक्ति नहीं होती। और अंततः ये सब भी हमारे देखने के तरीके मात्र ही हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। इस सब विवेचन की उपयोगिता केवल इतनी है कि इससे हमारी बुद्धि में कुछ अधिक प्रकाश आ जाता है। बाकी, अपने आप में सत्य तो इतना विशाल है कि किसी भी मानसिक सूत्र में उसे बाँधा ही नहीं जा सकता।
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
हिन्दैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्य तत् ॥ ५॥
५. अभिमान और मोह से विमुक्त जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, और जिनकी समस्त कामनाएँ शांत हो गयी हैं, जो सतत् रूप से आध्यात्मिक चेतना में प्रतिष्ठित हैं, जो सुख और दुःख के द्वन्द्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे वे अविमूढ़ जन उस अविनाशी परम पद की ओर अग्रसर होते हैं।
....जब तक मनुष्य गुणों की क्रीड़ा का भोग करता है तथा कामनाओं में लिप्स है तब तक वह प्रवृत्ति की कुण्डलियों में, जन्म और कर्म के प्रवाह में फंसा हुआ है, वह निरंतर भूलोक, मध्य के लोकों तथा स्वर्ग-लोकों के बीच चक्कर काटता रहता है तथा अपनी परमोच्च आध्यात्मिक अनंतताओं की ओर लौटने में समर्थ नहीं होता। ऐसा प्राचीन ऋषियों द्वारा भली-भाँति समझ लिया गया था। इसलिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए वे निवृत्ति या कर्म की मूल प्रेरणा के निरोध के मार्ग का अनुसरण करते थे और इस मार्ग की पराकाष्ठा है स्वयं जन्म का ही निरोध तथा सनातन की सर्वोच्च विश्वातीत भूमिका में परात्पर पद की प्राप्ति। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि कामना की इन दीर्घ काल से जमी जड़ों को अनासक्ति की प्रबल तलवार से काटना और फिर उस परम लक्ष्य की खोज करना जहाँ से, एक बार वहाँ पहुँच जाने के बाद, पुनः मर्त्य जीवन में लौटने की कोई बाध्यता नहीं रहती।
जब तक व्यक्ति कामनाओं, आसक्तियों में लिप्त रहता है तब तक वह संसार चक्र में फँसा रहता है। इसलिए प्रचलित तरीका रहा है कि किसी प्रकार इस जगत् प्रपंच से छूट निकलना, कर्म की मूल प्रेरणा अर्थात् कामना का ही निरोध करना और कामना के निरोध करने का अर्थ है स्वयं जन्म का ही निरोध करना। जब तक दिव्य कर्मों का रहस्य न प्राप्त हो गया हो, जब तक पुरुषोत्तम का रहस्य प्राप्त न हो गया हो जो क्षर और अक्षर दोनों में ही समान रूप से अपनी क्रिया करते हुए इन दोनों से ही परे बने रहते हैं, तब तक तो स्वयं जन्म का ही निरोध एक तर्कसंगत और उचित उपाय प्रतीत होता है। सच्चे कर्म तभी संभव हैं जब उनका उत्प्रेरण कामना के द्वारा नहीं अपितु भागवत् संकल्प के द्वारा हो। गीता आरंभ ही इसी से करती है कि 'तेरा कर्म का अधिकार है, कर्मफल का नहीं'। परंतु चूँकि दिव्य कर्म करना अत्यंत दुष्कर है इसलिए सहज ही व्यक्ति कर्मों के त्याग और यहाँ तक कि जीवन के ही निरोध की ओर प्रवृत्त होता है। हालाँकि स्वयं गीता कहती है कि बिना कर्म किये तो कोई रह ही नहीं सकता। एक पत्थर भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता। और कर्म केवल शरीरिक ही नहीं होते, अपितु प्राणिक और मानसिक भी होते हैं। इसलिए अकर्म संभव भी नहीं है और उसका कोई लाभ भी नहीं है। इसकी बजाय कर्मों को दूषित करने वाली चीज कामना को हटाकर दिव्य संकल्प के अनुसार कर्म करना ही सच्चा उपाय है। आरंभ में ये कामनारहित कर्म हमें अपने सच्चे भाव में आरोहण करने में सहायक होते हैं और उस स्थिति में प्रतिष्ठित होने के बाद उसकी अभिव्यक्ति के साधन बन जाते हैं। परंतु कर्मों को कामना से रहित करने के लिए भी इसके उपाय के रूप में गीता भगवान् की भक्ति को बताती है। भक्ति के द्वारा व्यक्ति को आनंद आने लगता है। उस आनंद के सहारे ही वह निम्न आनंद को छोड़ सकता है। यदि हम यह अपेक्षा करें कि व्यक्ति किसी उच्चतर आनंद की अनुभूति के बिना ही निम्नतर सुख को छोड़ दे तो यह संभव नहीं है। अतः जब व्यक्ति के अंदर भगवान् की भक्ति जागृत हो जाती है और उसे भगवान् के सत्स्वरूप में आनंद आने लगता है तब स्वतः ही कामनाओं पर धीरे-धीरे अंकुश लगने लगता है और अधिकाधिक वह अपने कर्म भगवान् के निमित्त करने लगता है क्योंकि ऐसा कर के उसे कामनाप्रेरित कर्मों की अपेक्षा अधिक आनंद आने लगता है।
हालाँकि जो निवृत्तिमार्गी थे उनके भी किसी एक भाग को तो कामना की पूर्ति से मिलने वाले सुख की अपेक्षा इस मार्ग पर अधिक संतोष मिलता था, परंतु इससे व्यक्ति के हृदय को, उसके प्राणिक भागों को, उसके सुखभोगवादी भागों को, मानसिकता को अपनी अभिव्यक्ति का कोई स्थान नहीं मिलता था और इससे उनकी कोई परिपूर्ति नहीं होती थी इसलिए वह एक बड़ा ही क्षुद्र और मर्यादित आनंद ही होता था। सारी सत्ता इस आनंद में भागीदार नहीं होती थी। इसी कारण किसी आत्मा विशेष के लिए तो अपने सभी भागों का निषेध करना उचित हो सकता है परंतु सामान्य रूप से यह कोई उचित मार्ग नहीं है। साथ ही अन्य भागों का दमन करके जो स्थिति प्राप्त की जाती है वह बड़ी हो संदिग्ध रहती है और उसे स्थायी बनाए रखने के लिए भी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। जबकि भक्ति के मार्ग में सारे ही भाग अपनी परिपूर्ति प्राप्त करते हैं और चूँकि इसमें व्यक्ति को अधिकाधिक आनंद प्राप्त होता है इसलिए उसे न तो किसी प्रकार के श्रम का अनुभव होता और न ही इस अवस्था को बनाए रखने में किसी प्रकार की तपस्या का अनुभव होता है। साथ ही अपनी अधिकतम परिपूर्ति होने के कारण हमारे सभी भागों का अभिव्यक्ति में आने का उद्देश्य भी सफल हो जाता है। अन्यथा यदि उनका दमन कर दिया जाए तब तो उन भागों का अभिव्यक्ति में आने का औचित्य ही नहीं रहता।
प्रश्न : 'उन परम् पुरुष का यह रहस्य ही प्रेम और भक्ति का गुप्त मर्म है।' तो यह कौन-सा रहस्य है जिसका यहाँ उल्लेख हुआ है?
उत्तर : इसके बारे में श्रीअरविन्द अठारहवें अध्याय में बड़े ही स्पष्ट रूप से निरूपण करते हैं। उनका कहना है कि परम पुरुष हमारी वैयक्तिकता और निर्वैयक्तिकता की मानसिक परिभाषाओं से सर्वथा परे हैं परंतु फिर भी वे कोई ऐसे अमूर्त और अनिर्देश्य नहीं हैं जिनसे कि कोई व्यक्तिगत संपर्क न साधा जा सके। उनका व्यक्तित्व अवश्य ही ऐसा है जिससे हम संपर्क साध सकते हैं, परंतु वह कोई सीमित व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक से सर्वथा परे वे एक परम पुरुष हैं। अब यदि परमात्मा केवल निर्वैयक्तिक सत्ता ही होते तब तो भक्ति की कोई संभावना ही नहीं रहती क्योंकि किसी अमूर्त सत्ता की हम भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं और न उससे कोई संपर्क ही साधा जा सकता है। साथ ही, मान लें कि परम पुरुष एक व्यक्तित्व हैं, परंतु तो भी यदि वे जीव के साथ कोई संपर्क साधने में रुचि न रखते हों तब तो जीव के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके सहारे वह उन तक पहुँच सके। इसलिए एक भक्तिमार्गी कहता है कि जिस प्रकार वह प्रभु को प्रेम करता है और उनमें आनन्द अनुभव करता है उसी प्रकार प्रभु भी अवश्य ही उससे प्रेम करते हैं और उसमें आनन्द लेते हैं और उससे मिलने के लिए लालायित रहते हैं और इसी कारण भक्त भगवान् से मिल पाता है। यदि भगवान् जीव में आनन्द अनुभव नहीं करते तब तो जीव अस्तित्व में ही नहीं आ सकता था। और चूंकि वे हमारे अंदर आनन्द अनुभव करते हैं इसीलिए हमें उनके प्रति आकर्षण महसूस होता है। इस आकर्षण के कारण ही प्रेमी और प्रेमास्पद का मिलन हो पाता है। इसी को उजागर करते हुए अपने ग्रंथ 'योग-समन्वय' में श्रीअरविन्द लिखते हैं कि, "प्रेम तथा आनंद सत्ता के चरम शब्द हैं, रहस्यों के रहस्य और गुह्यातिगुह्य हैं।"* अतः इस आनंद के लिए ही भगवान् ने इस सारे जगत् का निर्माण किया है। यदि परमात्मा केवल शांत और शाश्वत और अविचल निर्वैयक्तिक, अनिर्देश्य सत्ता ही होते तो हमारा उनसे किसी भी प्रकार संबंध स्थापित करना, उनसे संसर्ग करना, उनके प्रति अपने भाव आदि व्यक्त करना तो संभव ही नहीं होता क्योंकि किसी अमूर्त चीज के साथ कोई संबंध किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। श्रीअरविन्द के अनुसार तो शक्ति या ऊर्जा का ऐसा कोई रूप नहीं है जिसकी अपनी पृथक् सत्ता न हो। उनके अनुसार अचेतनता, अज्ञान आदि सभी की अपनी पृथक् पृथक् सत्ता होती है। श्रीमाताजी के अनुसार तूफान, अग्नि, वर्षा आदि सभी शक्तियों की अपनी-अपनी सत्ता होती है और इन सब का पृथक् व्यक्तित्व होता है। और चूँकि परम पुरुष केवल कोई अमूर्त सत्ता ही नहीं हैं अपितु मूर्त भी हैं और हमारे अंदर आनंद लेते हैं इसी कारण उनसे प्रेम करना, भक्ति करना, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना सर्वथा संभव ही नहीं अपितु एकमात्र करने योग्य कार्य है। भगवान् का यह रूप, उनसे यह संसर्ग ही वह सबसे शक्तिशाली माध्यम है जो जीव को भगवान् से एक कर देता है। इसी कारण हम कितने ही सिद्ध पुरुषों तथा भक्तों आदि की कथाओं में उल्लेख पाते हैं कि जिस विग्रह या मूर्ति की वे सेवा करते थे वह उनके लिए एक मूर्ति मात्र ही न रहकर भगवान् की एक जीवंत उपस्थिति बन जाती थी। श्रीकृष्णप्रेम सदा अपने चिरसाथी और इष्ट के रूप में कृष्ण की एक मूर्ति अपने साथ रखते थे। उनके अनुसार भक्ति भगवान् की अमूर्त या अकाल मूलसत्ता के रूप के प्रति उपासना नहीं है।
____________
* CWSA 24, p. 605
यह तो ईश्वर की जीवंत अभिव्यक्ति के प्रति मूर्त या ठोस प्रेम है। उनके अनुसार कृष्ण का विग्रह परम्-प्रभु का महज़ कोई प्रतीक नहीं अपितु उनकी मूर्तिमान् वास्तविकता है। श्रीरामकृष्ण द्वारा माँ काली की जीवंत प्रतिमा से संवाद करने और उससे सतत् मार्गदर्शन प्राप्त करने की बात से भी यही रहस्य प्रकट होता है। हमारे साहित्य में भी हम ऐसा वर्णन पाते हैं कि वे जो निराकार, अनिर्देश्य ब्रह्म हैं वे ही गोकुल में अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं। जिस निराकार का ध्यान लगा कर भी ऋषि-मुनि पार नहीं पाते वे ही नन्द के लाला के रूप में गोकुल में गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ नाचते हैं। अतः यह एक परम रहस्य है कि जो परमात्मा सब के नियंता, धारक, शासक, प्रतिपालक आदि हैं, वे ही प्रेमी के दास बन जाते हैं। ऐसी महिमा है प्रेम की।
भागवत् में भी बताया गया है कि और सब कुछ प्राप्त करना तो अपेक्षाकृत रूप से आसान है परन्तु भगवान की भक्ति प्राप्त करना सहज नहीं है। क्योंकि भक्ति के प्रभाव से तो भगवान् भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। कितनी ही कथा-कहानियों में हम पाते हैं कि भक्त के ऊपर भगवान् के कोई नियम प्रभावी नहीं होते। भक्त के प्रेम के लिए तो भगवान् नियम आदि सब पलट देते हैं। फिर तो वे वही करते हैं जो भक्त चाहता है।
अंत में गीता अर्जुन को भी यही उपदेश करती है कि सब कुछ छोड़ कर परमात्मा की शरण ग्रहण कर। और जिसे भी इसका जीवंत अनुभव है कि किस प्रकार भगवान् भी भक्त से प्रेम करते हैं वही जानता है कि सभी मानवीय भावों की सच्ची परिपूर्ति भगवान् के साथ प्रेम करने में ही होती है। ऐसा कोई भाव नहीं जिसका भगवान् अतिशय प्रेम के साथ उत्तर न देते हों, क्योंकि यदि भगवान् उन सभी मानवीय भावों को परितृप्त न कर सकते हों तब तो उन भावों का कोई औचित्य ही नहीं था। इसी कारण भक्तिमार्ग में हम अनेकानेक भावों का वर्णन पाते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति भगवान् के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। सकारात्मक ही नहीं, यहाँ तक कि द्वेष आदि नकारात्मक भावों के साथ भी भगवान् के चिंतन और उनसे संपर्क साधने की अनुमति दी गई है। श्रीकृष्ण के विषय में श्रीकृष्णप्रेम कहते हैं कि वे कोई निस्तेज अमूर्त या प्रतीक नहीं हैं, परंतु चाहे वे गोलोक में हों या इस जगत् में, वे तो सभी मूर्तताओं से अधिक मूर्त हैं। श्री दिलीप कुमार रॉय को एक पत्र में उन्होंने लिखा, "कुछ लोग 'उनका' वर्णन निराकार के रूप में या फिर हजारों हाथ-पैरों से युक्त के रूप में करते हैं परंतु मेरे लिए तो दो चरण ही पर्याप्त हैं। और अहा, क्या चरण हैं। यदि कोई इन्हें चूक जाता है तो कोई ब्रह्मानंद और कोई भी मुक्ति इस क्षति की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ लोग इसे मानव-आकारिता पुकारेंगे, परंतु वे क्या पुकारते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? तथ्य तो तथ्य हैं और इस आधुनिक धारणा को मैं अस्वीकार करता हूँ कि एकमात्र अमूर्तता ही सत्य है। जैसे कभी भी कोई आनंद नहीं हो सकता था यदि कृष्ण आनंदमय न होते, ठीक उसी प्रकार कहीं कोई मूर्तता नहीं होती यदि वे मूर्त न होते और कहीं कोई रूप न होता यदि उनका कोई रूप न होता। जैसा तुम जानते ही हो, एक समय मैं बुद्ध की पूजा करता था, और वह भी गहराई से; परंतु वह तो मेरे कृष्ण को जानने से पहले था, और अब, जब मैं अतीत के परिदृश्यों को देखता हूँ, तो सभी छायानुमा भूतहा आकृतियों की राशि के बीच मैं अलौकिक प्रकाश से जगमगाते उस एक दिव्य रूप को ही देखता हूँ। परंतु अतीत ही क्यों? भूत, वर्तमान और भविष्य, 'उनके' अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। 'उनके' श्रीविग्रह के वक्र और भंगिमाएँ तो सभी अनंतताओं, शाश्वतताओं और परम् तत्त्वों से अधिक मूल्यवान् हैं। समस्त लोक तो उनकी त्वचा के पौरों में समाए हैं, और तब भी वे कोई धुँधली-सी वैश्विक आकृति नहीं बने रहते, अपितु वे तो पीली धोती में, मोरपंख धारण किये, बाँस की बाँसुरी की धुन से आत्मा को मदमस्त कर देने वाले शाश्वत ग्वाला ही बने रहते हैं। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने (कृष्ण से परे भी कोई तत्त्व हो सकता है - मैं नहीं जानता)।" इस पत्र की प्रशंसा करते हुए श्रीअरविन्द ने लिखा, "दिलीप, हमेशा की ही तरह कृष्णप्रेम का पत्र शुरू से अंत तक सारगर्भित है; बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उनके पास एक जीवंत आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक ज्ञान है"। (योगी श्रीकृष्णप्रेम, पृष्ठ १७२-७३)
अतः जिन्हें परमात्मा की सत्ता का जीवंत अनुभव प्राप्त हो चुका है वे ही जानते हैं कि वे परम पुरुष होते हुए भी अभिव्यक्ति तथा संबंधों से परे नहीं हैं अपितु उनका संपर्क तो इतना मधुर और आनंददायक है कि सभी मानव भावों की सच्ची परिपूर्ति और परिणति उन्हीं में होती है। और यही परम रहस्य है। इसीलिए गीता अर्जुन को अठारहवें अध्याय में पहले कहती है कि उन ईश्वर की शरण ग्रहण कर जो यंत्र पर आरूढ़ के समान सभी भूतों को घुमाते रहते हैं और इससे तुझे शाश्वत पद और परा शांति प्राप्त होगी। परंतु इसके बाद भगवान् परम गुह्यतम वचन के रूप में अर्जुन को सभी कुछ का परित्याग करके अपनी शरण ग्रहण करने के लिए कहते हैं। यह आत्मा की एक ऐसी गति है जो सभी साधना और योग-पद्धतियों से परे है क्योंकि सभी योग-पद्धतियों का तो गीता ने इस वचन से पहले ही भली-भाँति निरूपण और समन्वय साध दिया होता है। परंतु सभी कुछ का निरूपण करने के बाद वह कहती है, 'सर्वधर्मान् परित्यज्य', क्योंकि वास्तव में यही एक सच्चा भाव है – अनन्य रूप से अपने-आप को भगवान् को सौंप देना। सामान्यतया जिन्हें हम साधना पद्धतियाँ कहते हैं वे कम या अधिक स्व-केंद्रितता लाती हैं और व्यक्ति को अपने अहं से बाँधे रखती हैं। इसीलिए भगवान् अर्जुन को सभी योग आदि की पराकाष्ठा या परिणति के रूप में कहते हैं 'सर्वधर्मान् परित्यज्य'। केवल प्रेम ही है जो अपने-आप को पूर्ण रूप से दे सकता है, अपने-आप को भुला सकता है। अन्य कोई साधना पद्धति भाव की ऐसी पराकाष्ठा तक नहीं ले जा सकती।
प्रश्न : पर ऐसा क्यों होता है कि एक बार आनन्द आने के बाद चला जाता है?
उत्तर : सच्चे प्रेम में ऐसा नहीं होता। परंतु यदि कोई प्राणिक आकर्षण या आसक्ति आदि का भाव हो तब उसमें आत्म-दान का भाव नहीं होता, वह तो केवल अपनी तुष्टि चाहता है। प्राण को विरह की पृष्ठभूमि पर मिलन सुखकर लगता है। एकरस मिलन से वह ऊब जाता है। इसी कारण हम विरह आदि की चर्चा सुनते हैं। परंतु ऐसे भाव का प्रेम से सरोकार नहीं होता। वह तो प्रेम के नाम पर प्राण की भगवान् को ही निगल जाने की प्यास होती है। प्राणिक भक्ति स्वयं पर ही केन्द्रित होती है। यदि एक बार यह सच्चा चैत्य प्रेम प्राप्त हो जाता है तब इसमें मिलन-विरह आदि नहीं होते। प्राणिक प्रेम में प्रेमी देना नहीं चाहता अपितु प्राप्त करना चाहता है। प्राणिक प्रेम का प्रत्युत्तर कम ही मिलता है और विरह की ही अधिकता होती है। इसमें प्रेमी भगवान् पर आधिपत्य जमाना चाहता है, उन्हें हस्तगत करना चाहता है जबकि चैत्य में ऐसा भाव नहीं होता। वह तो अपने-आप को दे देने के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। और ऐसा उसे कोई प्रयास करके नहीं करना पड़ता अपितु उसका स्वभावमात्र ही ऐसा है कि वह स्वतः ही भगवान् की ओर चलता है। और इस चैत्य प्रेम से ऊपर केवल एक ही अवस्था है और वह है परम पुरुष और उनकी परा-प्रकृति के बीच का अभिन्न परस्पर सम्बन्ध। ऐसा सम्बन्ध जिसमें वे दोनों एक ही हैं और यह ऐक्य प्रेम से भी परे है। इस प्रगाढ़ता की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह एक ऐसी शक्ति है जो असंख्यों ब्रह्माण्डों का निर्माण और उनका संचालन करती है। ये ही दो जब अभिव्यक्ति में आते हैं तब दिव्य प्रेम का रूप ले लेते हैं। इस दिव्य प्रेम के बिना रूपांतर साधित नहीं हो सकता। यही इस ब्रह्मांड का सबसे गुह्य रहस्य है।
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।। ६।।
६. उसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता, न चन्द्रमा और न ही अग्नि; वह मेरा परम घाम है, जिससे, जो वहाँ पहुँच जाते हैं वे, पुनः लौटकर नहीं आते।
...ऐसा प्रतीत होगा कि यह परम पद सम्यक् रूप से, यहाँ तक कि सर्वोत्तम रीति से, विशिष्ट और साक्षात् रूप से, संन्यास की निवृत्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति का नियत पथ अक्षर का मार्ग, अर्थात् कर्म और जीवन के पूर्ण त्याग, एक संन्यासमय एकांतवास, एक संन्यासमय निष्क्रियता का मार्ग प्रतीत होगा। यहाँ कर्म के आदेश के लिए अवकाश ही कहाँ है, अथवा कम-से-कम उसके लिए पुकार एवं आवश्यकता ही कहाँ है, और इस सबका लोकसंग्रह के साथ, कुरुक्षेत्र के संहार, कालपुरुष की गतिविधि के साथ, कोटि-कोटि-देहधारी ईश्वर के विराट्दर्शन तथा उनके इस उच्चघोषित आदेश के साथ क्या संबंध है कि, "उठ, शत्रु का वध कर, एक समृद्ध राज्य का भोग कर"? और फिर यह प्रकृतिगत पुरुष कौन है? यह पुरुष भी, यह क्षर, हमारी परिवर्तनशील सत्ता का यह भोक्ता भी पुरुषोत्तम ही है: गीता का उत्तर यह है कि अपने सनातन अनेकत्व में पुरुषोत्तम ही क्षर हैं।
धीरे-धीरे अब गीता पुरुषोत्तम तत्त्व के निरूपण की ओर गति करती है। गीता उसी को सभी कुछ के मूल के रूप में प्रतिपादित करती है। अतः क्षर की बजाय अक्षर की शांति में प्रतिष्ठित होने का उपदेश करने के बाद अब गीता क्षर और अक्षर दोनों के ही मूल पुरुषोत्तम भाव में जाने की ओर संकेत करती है।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।। ७।।
७. यह मेरा ही सनातन अंश है जो जीवों के इस लोक में जीव बनता है और प्रकृति में रहनेवाली छः इन्द्रियों को, जिनमें मन सम्मिलित है, आकृष्ट अथवा ग्रहण करता है।
यह एक ऐसा लक्षण, एक ऐसा कथन है जो एक बड़ा भारी अभिप्राय एवं महत्त्व अथवा परिणाम रखता है। क्योंकि इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यष्टि-पुरुष, अपने आध्यात्मिक सत्स्वरूप में साक्षात् भगवान् ही है, भले ही प्रकृति के अंदर वह वस्तुतः उन्हें कितने ही आंशिक रूप में क्यों न अभिव्यक्त करता हो। और, यदि शब्दों का कोई अर्थ हो तो, इसका यह भी अभिप्राय है कि अभिव्यक्त होनेवाली प्रत्येक आत्मा, अनेक में से प्रत्येक सनातन व्यष्टि है, एकं सत् की नित्य अजन्मा अमर शक्ति है। प्रकट होनेवाली इस आत्मा को हम जीव कहते हैं, क्योंकि यहाँ सजीव प्राणियों के जगत् में यह एक सजीव प्राणी प्रतीत होता है, और मनुष्य में अवस्थित इस आत्मा को हम मानव जीव कहते हैं और इसके विषय में केवल मानवता के तरीके से ही सोचते हैं। परन्तु वास्तव में यह ऐसा कुछ है जो अपनी वर्तमान प्रतीति से अधिक महान् है तथा अपने मानवीय रूप से आबद्ध नहीं है: अपने अतीत में यह मानव से कनिष्ठतर अभिव्यक्ति था, अपने भविष्य में यह ऐसा कुछ बन सकता है जो मनोमय मनुष्य से भी अत्यधिक महान् हो। और, जब यह जीव सब अज्ञानमय सीमाओं से ऊपर उठ जाएगा तब यह अपनी दिव्य प्रकृति धारण कर लेगा, जिसका कि इसका मानवीय रूप केवल एक अस्थायी आवरणमात्र है, आंशिक एवं अपूर्ण महत्त्व वाली वस्तु है। व्यष्टिगत आत्मा इस लोक के परे सनातन के अंदर अस्तित्वमान है और सदा ही अस्तित्वमान थी, क्योंकि वह स्वयं भी सनातन है। स्पष्टतः, जीव की सनातनता का यह विचार ही है जिसके कारण गीता ऐसे किसी भी कथन से बचती है जो किंचित्मात्र भी पूर्ण लय की ओर संकेत करता हो, अपितु उसने पुरुषोत्तम के अंदर निवास करने को ही जीव की सर्वोच्च स्थिति बताया है, निवसिष्यसि मय्येव । यद्यपि 'सबके एक आत्मा' के विषय में कहते समय वह अद्वैत की भाषा का प्रयोग करती प्रतीत होती है, तो भी सनातन व्यष्टि-जीव का यह नित्य सत्य, ममांशः सनातनः, ऐसा कुछ और जोड़ देता है जो एक विशिष्ट तत्त्व को ले आता है और लगभग विशिष्टाद्वैत के दर्शन को ही स्वीकार करता प्रतीत होता है, - हालाँकि इस कारण हमें एकदम इस परिणाम पर नहीं पहुँच जाना चाहिए कि बस वही गीता का एकमात्र दर्शन है या उसकी शिक्षा बाद के रामानुज के सिद्धांत के सर्वथा समान है। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि एकमेव भागवत् सत् की आध्यात्मिक सत्ता में बहुत्व का एक शाश्वत, केवल भ्रमात्मक ही नहीं, अपितु एक वास्तविक तत्त्व विद्यमान है।
यहाँ भगवान् जीव को अपना ही अंश बताकर सारे ही समीकरण को एक नया मोड़ प्रदान कर देते हैं। जिस जीव को क्षर और अनित्य, नश्वर आदि मानकर अवमानित किया जा रहा था और जिस अवस्था को हीन मानकर जिससे किसी भी भाँति छूट निकलकर अक्षर पुरुष में जाने की बात हो रही थी, भगवान् तो उसे अपना सनातन अंश बताकर सारे समीकरण को ही बदल डालते हैं। यदि जीव उन्हीं का सनातन अंश है जो सदा ही रहने वाला है तब तो जन्म-मृत्यु से छूट निकलने की बातें, मोक्ष आदि की बातें तो सब एकाएक ही अप्रासंगिक हो जाती हैं। पहले बड़े विस्तार से गीता त्रिगुणों से परे जाने की बात करती है, अक्षर की शांति में जाने की बात करती है, और फिर पुरुषोत्तम तत्त्व को ले आती है। इसके बाद यहाँ गीता एक नए तत्त्व का प्रवेश कराती है कि जीव तो भगवान् का ही सनातन अंश है। यदि ऐसा न होता तो जीव अस्तित्व में आ ही कैसे सकता था क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त तो अन्य किसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इससे हमें गीता के विकासक्रम की विलक्षणता देखने को मिलती है। वह सभी संभव दृष्टिकोणों और पद्धतियों को उनका समुचित मूल्य और स्थान प्रदान करते हुए विकसित करती है परंतु उन्हें अपने समन्वयकारी भाव के द्वारा सारी योजना में समन्वित कर लेती है जिससे कि वे अपना एकांगी स्वरूप छोड़ देते हैं और एक समग्र चीज का अंग बन जाते हैं।
कहने का अर्थ है कि गीता अब सारी चीज को अधिकाधिक पुरुषोत्तम भाव की ओर मोड़ती जा रही है और एक बिंदु पर आकर भगवान् अर्जुन को सर्वभावेन उनकी ओर मुड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में तो अन्य सभी चीजें बुद्धि के स्पष्टीकरण के लिए तो उपयोगी हो सकती हैं परंतु करने योग्य सच्चा काम तो यही है कि व्यक्ति समग्र रूप से, 'सर्वभावेन' और अनन्य रूप से भगवान् की ओर मुड़ जाए। यदि गीता को निवृत्ति की ओर ही मोड़ना होता तब तो अपने विश्वरूप दर्शन के बाद ही गीता अपनी शिक्षा का इस बात से उपसंहार कर सकती थी कि इस अनित्य संसार से किसी भी प्रकार निवृत्त होकर अक्षर की शांति में निवास करना ही सच्चा उपाय है। परंतु गीता का ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। गीता तो सभी धर्मों को विकसित करके अंततः उन्हें अतिक्रम करने और उन्हें त्याग कर भगवान् की शरण ग्रहण करने का उपदेश करती है। प्रत्येक अध्याय में गीता किन्हीं विशिष्ट तत्त्वों को उभार कर सामने लाती है परंतु भगवान् के प्रति भक्ति में वह सभी का समन्वय करती है।
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ।। ८।।
८. जब ईश्वर एक देह धारण करते हैं तब अपने साथ इन (इंद्रियों और मन) को ले आते हैं, और जब इस देह का परित्याग करते हैं तो वायु जिस प्रकार गंध को उसके स्रोतों से अपने साथ ले जाती है उसी प्रकार वे इनको अपने साथ लेकर चले जाते हैं।
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।
अधिष्ठाय मनश्वायं विषयानुपसेवते ॥ ९॥
९. श्रोत्र, चक्षु और स्पर्श, रसना और घ्राण और साथ ही मन पर अधिष्ठित होकर वे इंद्रिय-विषयों का उपभोग करते हैं।
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।। १० ।।
१०. शरीर से बाहर निकलते हुए हों या शरीर में निवास करते हुए, गुणों का उपभोग करते हुए हों या ग्रहण करते हुए हों, विमूढ़ जन (अंतर्यामी ईश्वर को) नहीं देखते; जिनके ज्ञानचक्षु हैं वे ही देखते हैं।
यह सनातन व्यष्टि-पुरुष भागवत् पुरुष से भिन्न अथवा किसी भी प्रकार से वस्तुतः उससे पृथक् नहीं है। यह स्वयं साक्षात् ईश्वर ही हैं जो अपने एकत्व से सनातन बहुत्व के द्वारा - क्या समस्त सत्ता अनंत के इस सत्य की ही अभिव्यक्ति नहीं है? – हमारे अंदर अविनाशी जीव के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं और जिन्होंने यह शरीर धारण किया है तथा जो जब यह नश्वर ढाँचा प्रकृति के तत्त्वों में विलीन होने के लिए उतार फेंका जाता है तो इससे बाहर निकल जाते हैं। वे मन तथा इंद्रियों के विषयों के उपभोग के लिए प्रकृति की आत्मनिष्ठ शक्तियों, मन तथा पाँच इंद्रियों, को अपने साथ लाते तथा विकसित करते हैं, और अपने निष्कासन के समय भी वे उन्हें साथ ले जाते हैं जैसे वायु किसी पुष्प-पात्र से सुगंधों को लेती जाती है। परन्तु ईश्वर तथा क्षर-प्रकृतिस्थ जीव की तदात्मता बाह्य प्रतीति के कारण हमसे छिपी हुई है तथा क्षर प्रकृति के चलायमान धोखों की भारी भरमार में खो गयी है। और, जो लोग अपने-आपको प्रकृति के रूपों, मानवता के रूप या किसी अन्य रूप के द्वारा परिचालित होने देते हैं वे इस एकत्व को कभी नहीं देख पायेंगे, अपितु मानव-तन में अवस्थित भगवान् की अवज्ञा और अवहेलना ही करेंगे। उनका अज्ञान भगवान् को उनके प्रविष्ट होने तथा बाहर निकलने या स्थित रहने तथा भोग करने एवं गुणों को धारण करने में अनुभव नहीं कर सकता, अपितु केवल वही चीज देखता है जो मन और इंद्रियों के लिए गोचर होती है, उस महत्तर सत्य को नहीं देखता जिसकी झलक केवल ज्ञान-चक्षु के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोग उनकी झलक पाने का प्रयास भी करें तो भी तब तक उन्हें उनकी झलक नहीं मिल सकती जब तक कि वे बाह्य चेतना की सीमाओं को दूर करना न सीख लें और अपने अंदर अपनी अध्यात्मसत्ता गठित न कर लें, मानो उसके लिए अपनी प्रकृति के अंदर एक रूप ही निर्मित न कर लें।
वास्तव में, जब हम यह सोचते हैं कि ईश्वर इस अभिव्यक्ति में, गुणों, द्वंदों आदि में फंसे हुए हैं तो यह एक मूलभूत रूप से ही असंगत बात है। संभव है कि चेतना की किसी अवस्था विशेष में व्यक्ति को यह बंधन या फँसाव महसूस हो, परंतु परमात्मा के लिए ऐसा कोई भी बंधन या फँसाव नहीं है। संभव है कि निवृत्तिमार्गियों की चेतना में यह फँसाव महसूस होता होगा इसीलिए वे संसार से वैराग्य और इसके त्याग की बातें करते हैं, परंतु जिनकी आत्मा में पलायन की वृत्ति न होकर भागवत् अभिव्यक्ति की ओर वृत्ति होती है, जैसी की गीता की है, तब उन्हें इस प्रकार का कोई बंधन या फँसाव महसूस नहीं होता। ऐसी आत्मा के लिए यह जगत् माया नहीं होता। और उसके लिए त्याग जैसी कोई चीज का अस्तित्व ही नहीं होता क्योंकि इस मार्ग पर चलने पर तो व्यक्ति के समक्ष अधिकाधिक भव्य निधियाँ खुलती जाती हैं और सदा ही आरोहण में उसे अधिकाधिक आनंद प्राप्त होता जाता है। इसलिए जब व्यक्ति को अधिकाधिक आनंद और अधिकाधिक परिपूर्णता प्राप्त हो रही हो तो उसे त्याग कैसे कहा जा सकता है। जब तक व्यक्ति को यह आभास होता है कि उसे किसी वस्तु का त्याग करने की आवश्यकता है तो इसका अर्थ है कि वास्तव में वह सच्चे मार्ग पर नहीं है क्योंकि सही मार्ग पर त्याग की किसी प्रकार की कोई संभावना ही नहीं होती।
त्याग, संन्यास, निवृत्ति आदि की बातें तो अहमात्मक तदात्मता के कारण आती हैं जबकि वास्तव में संपूर्ण विश्व में परम् प्रभु और उनकी पराप्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्वयं पराप्रकृति ही जीव बनती है और इस लीला में आती है। अतः देखने का सच्चा दृष्टिकोण तो यही है कि सभी कुछ परम प्रभु और उनकी पराप्रकृति की ही लीला है, हालाँकि ये भी तत्त्वतः अभिन्न रूप से एक ही हैं परंतु केवल अभिव्यक्ति के लिए दो रुख अपनाते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पराप्रकृति परम प्रभु की प्रसन्नता के निमित्त ही असंख्यों ब्रह्माण्डों का निर्माण करती है और ऐसी अद्भुत सृष्टि करती है और उन सभी रूपों में किसी भी प्रकार परम प्रभु को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है। इसीलिए श्रीमाँ व श्रीअरविन्द इस जगत् को मिथ्या नहीं बताते, उल्टे वे तो पार्थिव अभिव्यक्ति को ही दिव्य बनाने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। पांडिचेरी स्थित श्रीअरविन्द आश्रम इसका एक जीवंत प्रारूप प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार उन्होंने भागवत् साम्राज्य की स्थापना को केवल किसी आदर्श के रूप में ही नहीं छोड़ा अपितु सूत्र रूप में उसे चरितार्थ करके भी दिखाया है। कोई भी संवेदनशील सक्ति तुरंत ही देख सकता है कि वह कोई साधारण सृष्टि नहीं अपितु श्रीमाँ व श्रीअरविन्द द्वारा की गई दिव्य सृष्टि है। जब हम इस परिप्रेक्ष्य में गीता को समझने का प्रयास करते हैं तभी उसके व्यापक स्वरूप को और सर्वसमावेशी भाव को कुछ समझ पाते हैं अन्यथा प्रायः ही गीता की शिक्षा को बड़े ही संकीर्ण अर्थों में ले लिया जाता है और परस्पर विरोधी मतों में बाँट दिया जाता है।
प्रश्न : जब स्वयं भगवान् ही सभी कुछ कर रहे हैं तब तो कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती?
उत्तर : ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? पूरी सृष्टि में हम एक प्रकार का क्रम और व्यवस्था देखते हैं जिसमें हमें सदा ही कुछ चीजों को स्वीकार और ग्रहण करना होता है और कुछ चीजों को अस्वीकार करना होता है। अब यदि कोई अतिविशाल पहेली है और हमारी दृष्टि में पूरी पहेली एक साथ नहीं दिखाई दे सकती इसका यह अर्थ नहीं हो जाता कि उस पहेली के टुकड़े हम सुविधानुसार कहीं भी रख सकते हैं। और चूंकि हम एक ही दृष्टिपात में उसे नहीं देख पाते इसका यह अर्थ भी नहीं है कि पहेली असंबद्ध है। इसलिए कमी दृष्टि की है न कि उस पहेली की। सत्य का अर्थ ही यही है कि वह देश-काल-पात्र की समस्वरता के अनुसार ही अभिव्यक्त होता है। जैसे, कदाचित् पशुओं को मानव व्यक्तित्व असंबद्ध प्रतीत होता होगा परंतु मानव चेतना ही अपनी क्रियाओं को समझ सकती है, वैसे ही हम परमात्मा की क्रिया को समझ नहीं पाते।
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ।। ११ ।।
११. जो योगीजन यत्न करते हैं, वे उन ईश्वर को अपने भीतर स्थित देखते हैं; किन्तु जो अभी तक सचेतन नहीं हैं, जो आध्यात्मिक साँचे में गठित नहीं हुए हैं, वे यत्न करते हुए भी उन्हें नहीं देखते।
अपने-आप को जानने के लिए मनुष्य को कृतात्मा होना होगा, अर्थात् आध्यात्मिक साँचे में गठित एवं पूर्ण होना होगा तथा अध्यात्म-दृष्टि में प्रबुद्ध होना होगा। जिन योगीजनों के पास यह ज्ञानचक्षु है वे अपने अनंत सत्स्वरूप में, अपनी आत्मा की शाश्वतता में हमारे वास्तविक स्वरूप भागवत् पुरुष के दर्शन करते हैं। ज्ञानदीप्त होकर वे प्रभु का अपने अंदर साक्षात्कार करते हैं और स्थूल जड़भौतिक सीमा से, मानसिक व्यक्तित्व के रूप तथा नश्वर प्राणिक रचना से मुक्त हो जाते हैं: वे आत्मा और अध्यात्म-सत्ता के सत्य में अमर होकर निवास करते हैं। परन्तु वे केवल अपने अंदर ही नहीं, अपितु समस्त सृष्टि में भी उनके दर्शन करते हैं।
प्रश्न : यहाँ श्रीअरविन्द टिप्पणी करते हैं कि 'मनुष्य को कृतात्मा होना होगा', तो क्या ऐसा करना मनुष्य के अपने हाथ में है?
उत्तर : मनुष्य के अंदर संभावना तो अवश्य ही निहित रहती है। कुछ जो अधिक परिपक्व होते हैं वे जब किसी सद्गुरु के संपर्क में आते हैं, या फिर अन्य किसी माध्यम से वे उस निहित संभावना के संपर्क में आ जाते हैं तब वे अपने सच्चे उद्देश्य को कुछ-कुछ पहचान जाते हैं और जीवन में उस ओर उनकी गति आरंभ हो जाती है। जिनमें अभी उतनी परिपक्वता नहीं है उनका भी सत्संग आदि से विकास हो सकता है। परंतु जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रख दिये हैं उनमें भी हजारों में से किसी एक को ही सच्ची अनुभूति प्राप्त होती है। अतः इसमें यह समझने की बात है कि हमारी सत्ता के अंदर अनेकानेक भाग हैं। यदि किसी भाग को आदेश या संपर्क प्राप्त हो भी गया है तो भी अनेकानेक ऐसे भाग शेष रह जाते हैं जिन्हें उस ओर जाने में कोई रुचि नहीं होती और वे अपने ही तय ढरें में चलते रहना चाहते हैं और अपने ही क्षुद्र हेतुओं की पूर्ति में रत रहते हैं। इसीलिए जब समय-समय पर हमारी सत्ता के ये सभी भाग सतह पर आते हैं तो कम या अधिक समय के लिए अंधकार के काल आ जाते हैं जिनके प्रति साधक को सचेतन होकर उन्हें पार करना होता है। एक दृष्टिकोण से यह आवश्यक भी है क्योंकि यदि ये भाग सतह पर न आते तो व्यक्ति इनके विषय में कभी सचेतन ही न होता और इस कारण से उनका शुद्धिकरण और रूपांतर भी न हो पाता। इसीलिए पूर्ण चैत्य अनुभूति होने के बाद भी तमाच्छादन के काल आ सकते हैं। इतना अवश्य है कि उन अंधकार के कालों में भी व्यक्ति को किसी ऐसी चीज की स्मृति बनी रहती है जिसके सहारे वह उनमें से निकल पाता है। साथ ही, एक सच्चे दृष्टिकोण में ये प्रकाशपूर्ण और अंधकारमय काल आत्मा का पोषण करने वाली दो माताओं के समान काम करते हैं जिन दोनों के ही द्वारा आत्मा परिपुष्ट होती है। परंतु गीता के वर्णन को पढ़कर यह नहीं समझ लेना चाहिये कि गीता जिस कृतात्मा होने की बात कर रही है वह कोई सीधी-सादी बात है। वह एक बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है और बिना गुरु के मार्गदर्शन के प्रायः इसे समझना संभव भी नहीं है।
साथ ही हमें समझना चाहिये कि यदि मूलतः व्यक्ति आध्यात्मिक साँचे में गठित नहीं होता तो प्रायः ही आध्यात्मिक मार्ग की ओर वह उद्घाटित नहीं हो सकता था। यदि भीतर से वह गठन आध्यात्मिक रूप का न हो तो जो चीजें किसी एक के लिए आध्यात्मिक मार्ग का उद्घाटन कर देती हैं वे ही उस व्यक्ति के लिए निष्प्रभावी रहेंगी और वह कदाचित् उन पर कोई ध्यान ही नहीं देने वाला। जो पुस्तक या मूर्ति, या फिर कोई गुरु जिससे किसी एक को साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है, वही आवश्यक नहीं कि किसी दूसरे के लिए कारगर सिद्ध हो। जो आध्यात्मिक साँचे में गठित होता है वास्तव में तो वही इस पथ पर आता है।
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते ऽखिलम् ।
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ।। १२ ।।
१२. सूर्य का जो प्रकाश सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करता है, चन्द्रमा में जो प्रकाश है और अग्नि में जो प्रकाश है उसे मेरा ही प्रकाश जान।
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।। १३।।
१३. मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने बल के द्वारा समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और (पृथ्वीमाता में) रस-रूप सोमदेव होकर समस्त पेड़-पौधों और औषधियों का पोषण करता हूँ।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ।। १४।।
१४. मैं प्राण-रूप अग्नि (वैश्वानर) होकर, सजीव प्राणियों की देह में आश्रित होकर तथा प्राण और अपान वायु से युक्त होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ।
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ।। १५।।
१५. मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मुझ से ही स्मृति, ज्ञान और उनका अभाव उत्पन्न होते हैं। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य एकमेव हूँ, मैं ही वेदान्त का रचयिता और वेद का ज्ञाता हूँ।
दूसरे शब्दों में, भगवान् एक ही साथ जड़तत्व की आत्मा, प्राण की आत्मा, मन की आत्मा हैं तथा उस अतिमानसिक ज्योति की भी आत्मा है जो मन और इसकी संकीर्ण तर्कबुद्धि से परे है।
धीरे-धीरे अब हम गीता के स्वर में एक निर्णायक भेद पाते हैं। जहाँ पहले निषेधात्मक स्वर था वहीं अब भगवान् स्पष्ट रूप से अपनी सत्ता को अधिकाधिक प्रतिष्ठित करते जा रहे हैं और कहते हैं कि सभी कुछ वे ही हैं। वे ही शरीर धारण कर इंद्रियों और मन को अपने साथ लाते हैं, वे ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य एकमेव हैं; वे ही वेदान्त के रचयिता और वेद के ज्ञाता हैं, स्वयं वे ही सभी अन्नों को पचाते हैं। जो कुछ भी अभिव्यक्ति में आया है वह सभी कुछ इस अर्थ में भगवान् स्वयं ही हैं कि सभी कुछ एकमात्र पराप्रकृति द्वारा ही अभिव्यक्त होता है और पराप्रकृति की अपने-आप में प्रभु से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परम प्रभु और उनकी पराप्रकृति तो अभिन्न रूप से एक ही हैं।
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्वाक्षर एव च ।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।। १६।।
१६. इस लोक में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं; क्षर पुरुष इन सभी भूतों के रूप में है; और कूटस्थ (स्थिर और उच्चासीन) अक्षर पुरुष कहलाता है।
अतः, ये दोनों (क्षर और अक्षर) ही दो पुरुष हैं जिन्हें हम इस जगत् में देखते हैं; एक तो इसके कर्म में सामने की ओर प्रकट होता है, दूसरा पीछे की ओर उस शाश्वत शांति में दृढ़ रूप से अवस्थित रहता है जिससे कर्म निःसूत होता है और जिसमें सब कर्म कालातीत सत्ता, निर्वाण, के अंदर समाप्त हो जाते हैं और विलीन हो जाते हैं...
परंतु जो समस्या हमारी बुद्धि को चकरा देती है वह यह है कि ये दोनों ऐसे असमाधेय परस्पर-विरोधी प्रतीत होते हैं जिनमें कोई वास्तविक संयोजक कड़ी नहीं है और न ही इन दोनों में किसी एक से दूसरे पर पहुँचने के लिये विच्छेद की कोई अनुदार गति को छोड़कर और कोई साधन ही है। क्षर कर्म करता या, कम-से-कम, कर्म का उत्प्रेरण करता है, अक्षर में भी उससे पृथक् रहकर कर्म करता है; अक्षर अलग-थलग, आत्म-केंद्रित तथा अपनी निष्क्रियता में क्षर से पृथक् रहता है।.।...जब हम भूतभाव की अस्थिरता या गतिशीलता में निवास करते हैं तब हम कालातीत स्वयंभू सत्ता के अमृतत्व से सज्ञान भले ही हों, पर उनमें निवास कदाचित् ही करते हैं। और जब हम अपने-आप को कालातीत सत्ता के अंदर सुप्रतिष्ठित कर लेते हैं तब देश, काल और घटना सभी हमसे दूर हो जाते हैं और अनंत के अंदर एक विक्षुब्ध स्वप्न प्रतीत होने लगते हैं। अतएव, प्रथम दृष्टि में, सर्वाधिक विश्वासोद्पादक निष्कर्ष यह प्रतीत होगा कि प्रकृति के अंदर आत्मा की गतिशीलता एक भ्रम है, एक ऐसी चीज है जो केवल तभी सत्य है जब हम इसमें निवास करते हैं, पर जो तत्त्वतः सत्य नहीं है, और इसी कारण जब हम आत्मा के अंदर लौटते हैं, यह हमारे अविकार्य मूलतत्त्व से दूर हो जाती है। यही तो उस असमाधेय जटिल पहेली को सुलझाने का सुपरिचित तरीका है, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या।
गीता इस समाधान का आश्रय नहीं लेती, क्योंकि उक्त भ्रम की व्याख्या करने में इसकी असमर्थता के अतिरिक्त इस समाधान में स्वयं में बड़ी भारी समस्याएँ हैं, – क्योंकि यह तो केवल इतना ही कहता है कि यह सब एक रहस्यमय और अगम या दुरूह माया है, और तब उसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि यह सब रहस्यमय और अगम दोहरी यथार्थता है, आत्मा अपने को आत्मा से छिपाये हुए है। गीता माया की चर्चा तो करती है, पर केवल इस रूप में कि वह एक भ्रमोत्पादक अपूर्ण चेतना है जो पूर्ण यथार्थ तत्त्व को पकड़ नहीं पाती तथा अस्थिर गतिशील प्रकृति के प्रपंच में निवास करती है और जिस परम् आत्मा की यह सक्रिय शक्ति है, मे प्रकृतिः, उसकी इसे कोई झलक तक प्राप्त नहीं है। जब हम इस माया को पार कर जाते हैं तो यह जगत् लुप्त नहीं हो जाता, यह केवल अपने अंतरतम अर्थ में बदल जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में हमें जो कुछ पता चलता है वह यह नहीं कि इस सब जगत् का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अपितु यह पता चलता है कि इस सबका अस्तित्व तो है, पर इसके वर्तमान भ्रांत अर्थ से सर्वथा भिन्न, इसका एक दूसरा ही आशय हैः सब कुछ ही भगवान् है, आत्मा है, उसी की जीव-सत्ता और उसी की प्रकृति है, सब ही वासुदेव है। गीता के लिए यह जगत् वास्तविक है, ईश्वर की सृष्टि, सनातन की शक्ति तथा परब्रह्म से हुई अभिव्यक्ति है, और यहाँ तक कि त्रिगुणमयी माया की यह निम्नतर प्रकृति भी परा दैवी प्रकृति से उद्भूत हुई है।...गीता इस पर बल देती है कि हम अपने जीवनकाल में ही आत्मा तथा उसकी नीरवता में सचेतन रूप से रह सकते हैं और फिर भी प्रकृति के जगत् में शक्तिशाली रूप से कार्य कर सकते हैं एवं हमें इस प्रकार रहना तथा करना भी चाहिए। और, वह स्वयं भगवान का दृष्टांत देती है जो जन्म की अनिवार्यता से बंधे नहीं हैं, अपितु स्वतंत्र हैं तथा सृष्टि से उच्चतर हैं और फिर भी नित्य-निरंतर कर्म में रत रहते हैं, वर्त एवं च कर्मणि। अतः दैवी प्रकृति के साथ पूर्ण रूपेण साधर्म्य लाभ करने से ही इस द्विविध अनुभव की एकता पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है। परन्तु उस एकता का मूल तत्त्व क्या है?
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ।। १७।।
१७. इन दोनों से भिन्न एक उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है, को अविनाशी ईश्वर है और जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उन्हें धारण करता है।
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। १८ ।।
१८. चूंकि मैं क्षर से परे हूँ और अक्षर से भी महान् और उच्च हूँ, इसलिये वेद में और लोक में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ।
(एकता के इस मूल तत्त्व को) गीता पुरुषोत्तम-विषयक अपने परमोच्च दर्शन में प्राप्त करती है; क्योंकि उसके मत में यही पूर्ण और सर्वोच्च प्रकार का अनुभव है, यह पूर्ण ज्ञानी लोगों, कृत्स्नविदः, का ज्ञान है। अक्षर परम्, पर, हैं, विश्व-प्रकृति की सभी वस्तुओं तथा समस्त कर्म के संबंध से वे परमोच्च सत्ता हैं। वे सबके अक्षर आत्मा हैं, और सबके अक्षर आत्मा हैं पुरुषोत्तम। उनकी अपनी प्रकृतिगत शक्ति के कर्म से अप्रभावित, उनकी अपनी संभूति को प्रेरणा से अक्षत, उनके अपने गुणों की क्रीड़ा से अविचलित उनकी जो स्वयंस्थित सत्ता है उसकी स्वतंत्रता में वे (पुरुषोत्तम) अक्षर हैं। परंतु यह तो समग्र ज्ञान का केवल एक ही पहलू है, यद्यपि है एक महान् पहलू। इसके साथ ही पुरुषोत्तम अक्षर से भी अधिक महान् हैं, क्योंकि वे इस अक्षर भाव से अधिक कुछ हैं और वे अपनी सत्ता के सर्वोच्च नित्य धाम, परं धाम के द्वारा भी परिसीमित नहीं हैं। तो भी, हमारे अंदर जो कोई अक्षर एवं नित्य तत्व है। उसी के द्वारा हम उस सर्वोच्च धाम को प्राप्त करते हैं जहाँ से पुनः जन्म लेने के लिए नहीं लौटना पड़ता, और यही वह मोक्ष था जिसे पुराकाल के ज्ञानीजन एवं प्राचीन ऋषि-मुनि खोजा करते थे। परन्तु जब केवल अक्षर के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न किया जाता है तो वह यत्न अनिर्देश्य की खोज का रूप धारण कर लेता है, जो कि हमारी प्रकृति के लिए एक कठिन कार्य है, क्योंकि हम यहाँ जड़प्रकृति में देह धारण किये हुए हैं। वह अनिर्देश्णा, जिसकी ओर अक्षर, अर्थात् यहाँ हमारे अंदर विराजमान शुद्ध अगोचर आत्मा, अपने भेदमूलक आवेग के साथ ऊपर उठती है. कोई परम अव्यक्त सत्ता है, पररोऽव्यक्तः, और वह उच्चतम अव्यक्त अक्षर भी पुरुषोत्तम है। इसलिए भगवान् कहते हैं कि जो लोग अनिर्देश्य का अनुसरण करते हैं वे भी मुझ, सनातन परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। परन्तु फिर भी वे परमेश्वर उच्चतम अव्यक्त अक्षर से भी अधिक हैं, किसी भी निषेधात्मक निरपेक्ष तत्त्व, नेति, नेति से अधिक हैं, क्योंकि उन्हें उन उत्तम या परम् पुरुष के रूप में भी जानना होगा जो इस संपूर्ण ब्रह्माण्ड को अपनी ही सत्ता के अंदर विस्तारित करते हैं। वे परम रहस्यमय सर्व हैं, यहाँ की सब वस्तुओं के मूलभूत अनिर्वचनीय निरपेक्ष सत् हैं। वे क्षर में विद्यमान ईश्वर हैं, केवल वहीं नहीं, अपितु यहाँ प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान पुरुषोत्तम हैं, ईश्वर हैं। और वहाँ अपने नित्य परम पद, परो अव्यक्तः में भी परमेश्वर हैं, कोई अलग-थलग अथवा उदासीन और संबंध- रहित अनिर्देश्य नहीं, अपितु जीव और जगत् के उद्गम, माता-पिता, आदि मूल तथा नित्य आश्रय हैं, सर्वभूतों के स्वामी तथा यज्ञ और तप के भोक्ता हैं। उन्हें अक्षर और क्षर दोनों रूपों में एक साथ जानकर, उन अजन्मा के रूप में जानकर जो प्राणीमात्र के जन्म में अपने को अंशतः प्रकट करते हैं और यहाँ तक कि स्वयं भी सनातन अवतार के रूप में अवतीर्ण होते हैं, उन्हें उनके समग्र रूप में, समग्रं माम्, जानकर ही जीव निम्नतर प्रकृति के बाह्य रूपों से सुगमतया मुक्त हो सकता है तथा एक बृहत् आकस्मिक विकास एवं विशाल अपरिमेय आरोहण के द्वारा दिव्य सत् और पराप्रकृति में लौट सकता है। क्योंकि क्षर का सत्य भी पुरुषोत्तम का सत्य है।
इस प्रकार भगवान् अपनी रहस्यमय दोहरी आत्मा में, अपनी द्विविध शक्ति में प्रकट हैं, द्वाविमौ पुरुषौ; वे एक ही साथ क्षर वस्तुओं की उस आत्मा को धारण करते हैं जो ये सब भूत है, क्षरः सर्वाणि भूतानि, तथा उस अक्षर आत्मा को भी धारण करते हैं जो सर्वभूतों के ऊपर उनकी शाश्वत नीरवता और स्थिरता की अक्षुब्ध अचलता में स्थित रहती है। और इनके अंदर विद्यमान भागवत् शक्ति के कारण ही मनुष्य के मन, हृदय और संकल्पशक्ति इन दो आत्माओं के द्वारा विभिन्न दिशाओं में इतनी प्रबलता के साथ खींचे जाते हैं मानो ऐसे दो विरोधी एवं विसंगत आकर्षणों के द्वारा खींचे जा रहे हों जिनमें से प्रत्येक दूसरे को विनष्ट करने पर तुला हुआ है। परन्तु भगवान् न तो पूर्ण रूप से क्षर हैं और न पूर्ण रूप से अक्षर ही हैं। वे अक्षर पुरुष से महान् हैं और परिवर्तनशील (क्षर) वस्तु-समूह की आत्मा से भी अत्यधिक महान् हैं। यदि वे एक साथ दोनों ही भावों में बने रहने में समर्थ हैं तो इसका कारण यह है कि वे दोनों से अन्य हैं, अन्यः, समस्त सृष्टि के ऊपर अवस्थित पुरुषोत्तम हैं और फिर भी इस जगत् में व्याप्त हैं और साथ ही, वेद विश्वानुभूति में भी व्यापे हुए हैं।
हालाँकि दूसरे ही अध्याय से गीता में क्षर और अक्षर का उल्लेख , आत्म-ज्ञान तथा आता रहा है परंतु यहाँ गीता ने बडे ही निर्णायक रूप से इनसे ऊपर आता रत उत्तम पुरुष का उल्लेख किया है। गीता के स्वर में अब हम अधिकाधिक एक मूलभूत अंतर पाते हैं कि भगवान् अपनी सत्ता को स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आरंभ में भगवान् ने परोक्ष रूप से ही अपनी सत्ता का संकेत किया था, परंतु यहाँ स्पष्ट रूप से अपने को पुरुषोत्तम रूप से प्रतिष्ठित करके वे प्रत्यक्ष रूप से ऐसा उद्घोषित करते हैं। कि एकमेव उन्हीं की सत्ता है और वे ही सभी चीजों के एकमात्र कारण हैं, वे ही एकमेवाद्वितीय हैं। इतने स्पष्ट रूप से निरूपण के बाद भी हम गीता पर अनेकानेक टीकाएँ पाते हैं कि गीता क्षर भाव को त्याग कर अक्षर में अवस्थित होने की बात कहती है। कुछ मत गीता को कर्मों से संन्यास का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ बताते हैं। इसीलिए श्रीअरविन्द अपनी टीका के माध्यम से गीता की ही वाणी और अधिक प्रखर और असंदिग्ध बना देते हैं कि अक्षर में चले जाना उपाय नहीं है। सच्चा उपाय है पुरुषोत्तम की चेतना से तादात्म्य स्थापित करना क्योंकि पुरुषोत्तम की चेतना ही क्षर और अक्षर दोनों भावों को अपने उचित उपयोग में लाकर उन दोनों से ही परे बनी रहती है। वे एकमेवाद्वितीय परमात्मा ही अभिव्यक्ति में इतने असंख्य रूप धारण कर लेते हैं क्योंकि किसी एक रूप में तो उन्हें बाँधा ही नहीं जा सकता और इससे भगवान् की परम् स्वतंत्रता का भान होता है। हम परमात्मा पर जो भी गुण आरोपित करते हैं वे उनसे सर्वथा विपरीत पहलू भी अपना कर अपनी पूर्ण निरपेक्ष स्वतंत्रता का परिचय देते हैं। यदि हम उन्हें सर्वज्ञ की संज्ञा दें तो वे घोर अज्ञानी का रूप भी धर सकते हैं, यदि हम उन्हें सर्वशक्तिमान् की संज्ञा दें तो वे एक ऐसे क्षणभंगुर जीव का रूप भी धारण कर सकते हैं जिसका अस्तित्व मात्र ही सदा संदिग्ध रहता है। यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन सभी विपर्ययों के द्वारा हमें भगवान् की पूर्ण स्वतंत्रता का भान होता है। यही नहीं, वे हमारी स्वतंत्रता और बाध्यता की परिकल्पना से भी सर्वथा परे हैं।
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ।। १९।।
१९. हे भारत। मोहरहित जो मनुष्य इस प्रकार मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जनता एवं देखता है वह सर्व-ज्ञाता अपनी प्राकृत सत्ता के हर रूप, हर प्रकार से मेरी भक्ति करता है।
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।। २० ।।
२०. हे निष्पाप अर्जुन! इस प्रकार यह गुह्यतम शास्त्र मेरे द्वारा तुझे कहा गया है। हे भारत! इसे पूर्णतया जानने का अर्थ है बुद्धि में पूर्ण होना और परम अर्थ में सफल होना।
जो कोई भी उन्हें इस प्रकार पुरुषोत्तम के रूप में जानता तथा देखता है, वह फिर चाहे यह जगत्-दृश्य हो या फिर इन दो परस्पर विरोधी सत्ताओं का पृथक् आकर्षण हो, इनमें से किसी से भी फिर विभ्रांत नहीं होता।... वह उनका आलिंगन करता हुआ उन्हें अतिक्रांत कर जाता है, उनके विरोध को जीत कर सर्वविद्, समग्र-ज्ञानी बन जाता है। वह आत्मा और वस्तुओं का, दोनों का संपूर्ण आशय जान लेता है; वह भगवान् के समग्र सत्य को पुनः प्राप्त कर लेता है, समग्रं माम्: वह क्षर और अक्षर दोनों को पुरुषोत्तम में एकीभूत कर देता है। वह अपनी सत्ता तथा समस्त भूतों की सत्ता की परम् आत्मा से, अपनी शक्ति तथा सब शक्तियों के एकमात्र प्रभु से, जगत् में तथा इसके परे विद्यमान समीपस्थ और दूरस्थ सनातन से प्रेम करता, उनकी पूजा करता, उनकी शरण लेता तथा उनका भजन करता है। और, यह सब भी वह अपनी सत्ता के किसी एक ही पार्श्व या अंश के द्वारा, एकमात्र आध्यात्मीकृत मन, हृदय की चौंधियानेवाली प्रखर परंतु संकीर्ण ज्योति या केवल कर्मगत संकल्प की अभीप्सा के द्वारा नहीं, अपितु अपनी सत्ता एवं संभूति, अपनी आत्मा एवं प्रकृति के सभी सुप्रदीप्त साधनों के द्वारा, सर्वभाव से करता है। अपनी अविचल स्वप्रतिष्ठ सत्ता की समता में भगवत्स्वरूप होता हुआ तथा उस समता में सब पदार्थों एवं प्राणियों के साथ एकमय होता हुआ वह उस निःसीम समता तथा गंभीर एकत्व को अपने मन, हृदय, प्राण और शरीर के अंदर उतार लाता है और उसकी नींव पर दिव्य प्रेम, दिव्य कर्म एवं दिव्य ज्ञान के त्रैत को अविभाज्य एवं समग्र रूप में स्थापित करता है। गीता के मोक्ष का मार्ग यही है।
और आखिरकार क्या यही वह सच्चा अद्वैत नहीं है जो एकमेव सनातन सत् में लेश मात्र भी भेद नहीं करता? यह चरम भेदशून्य अद्वैतवाद एकमेव को प्रकृति की अनेकताओं में भी एक ही देखता है, यह उसे सब पहलुओं में एक ही देखता है, आत्मा तथा जगत् के सत्स्वरूप में भी वह उसे उतना ही एक देखता है जितना कि विश्वातीत के उस महत्तम सत्स्वरूप में जो आता का मूल तथा जगत् का सत्य है और जो न तो विश्व-संभूति की किसी प्रकार की सत्यता से या किसी वैश्विक अथवा निरपेक्ष निषेध से ही बद्ध होता है। कम-से-कम गीता का अद्वैत तो यही है। श्रीगुरु अर्जुन से कहते हैं कि यह परम गुह्य शास्त्र है; यह परम ज्ञान और विज्ञान है जो हमें सत्ता के उच्चतम रहस्य के मर्म में ले जाता है। इसे पूर्ण रूप से जानने तथा ज्ञान में, संवेदन में शक्ति एवं अनुभूति में इसे अधिकृत करने का अर्थ है रूपांतरित बुद्धि में पूर्ण होना, हृदय में दिव्य रूप से संतृप्त होना तथा समस्त संकल्प एवं कर्म-कलाप के परम प्रयोजन और उद्देश्य में कृतकृत्य होना। अमर होने, दिव्य परम प्रकृति की ओर ऊपर उठने तथा सनातन धर्म को धारण करने का यही मार्ग है।
इस प्रकार पंद्रहवाँ अध्याय 'पुरुषोत्तमयोग' समाप्त होता है।
--------------------------------------
* हमें मोक्ष की खोज क्यों करनी चाहिये इसका सब से अधिक यथार्थ कारण व्यक्तिगत रूप से जगत् के दुःख से मुक्त हो जाना नहीं है, - यद्यपि वह मुक्ति भी हमें प्राप्त होगी ही, - वरन् यह है कि हम भगवान्, पुरुषोत्तम और शाश्वत के साथ एक हो जायें। पूर्णता, अर्थात् परम स्थिति, पवित्रता, ज्ञान, बल, प्रेम और सामर्थ्य, की खोज हमें क्यों करनी चाहिए इसका सबसे अधिक यथार्थ कारण यह नहीं है कि व्यक्तिगत रूप में हम दिव्य प्रकृति का उपभोग करें, यह भी नहीं कि हम देवताओं के समान बन जायें, - यद्यापि ऐसा दिव्य उपभोग भी हमें अवश्य प्राप्त होगा, - वरन् यह ह है कि इस मुक्ति और पूर्णता को प्राप्त करना ही हमारे अन्दर भगवान् की इच्छा है, यही प्रकृति में हमारी आत्मा का सर्वोच्च सत्य है, यही विश्व में वर्द्धनशील अभिव्यक्ति का सदा-अभिप्रेत लक्ष्य है। स्वतन्त्र, सर्वागपूर्ण और आनन्दमयी दिव्य प्रकृति को व्यक्ति में अवश्य प्रकट होना चाहिये जिससे कि यह संसार में भी अभिव्यक्त हो सके। अविद्या (की अवस्था) में भी व्यक्ति वस्तुतः विराट् के अन्दर और विराटू के प्रयोजन के लिये ही निवास करता है क्योंकि अपने अहं के प्रयोजनों और कामनाओं का अनुसरण करता हुआ भी वह विश्वप्रकृति के द्वारा बाध्य होकर अपने अहंमूलक कार्य से इन लोकों के अन्दर उसी (प्रकृति) के कार्य और प्रयोजन में ही सहयोग देता है। परन्तु यह सहयोग वह बिना सचेतन संकल्प के एवं अपूर्ण ढंग से और उसकी अर्थ-विकसित एवं अर्द्ध-वेतन तथा अपूपेत एक संकल्प के एवं अपूर्ण हग हो अहं से मुक्त चोकू लागवान से एकत्व प्राप्त करना उसके व्यक्तिभाव का मुक्ति है और यही उसकी परिपूर्णता भी है। इस प्रकार मुक्त, शुद्ध और पूर्णता प्राप्त को मुक्ति दैन्य आत्मा - जैसा प्रारका से ही अभिमत था, सचेतन तथा समय रूप में, विराद और पररात्पर भगवान् में और उसके लिये तथा उसके विश्वगत संकल्प के लिये जीवन यापन करने लगता है।
सोलहवाँ अध्याय
देव और असुर
गीता की विचारधारा का विकास एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच गया है जहाँ केवल एक ही प्रश्न समाधान के लिए बाकी रह जाता है, - हमारी बद्ध और दोषपूर्ण प्रकृति का प्रश्न, कि केवल सिद्धान्त-रूप में ही नहीं अपितु अपनी सभी चेष्टाओं में, निम्नतर से उच्चतर सत्ता की ओर तथा अपने वर्तमान कर्म-विधान से शाश्वत धर्म की ओर यह अपना विकास किस प्रकार साधित कर सकती है। यह एक ऐसी समस्या है जो गीता-प्रतिपादित कुछ एक सिद्धान्तों में अंतर्निहित है, किन्तु जितनी प्रधानता उसे वहाँ दी गई है उसकी अपेक्षा अधिक प्रधानता के साथ निरूपित करने तथा अधिक स्पष्ट रूप में हमारी बुद्धि के समक्ष रखने की आवश्यकता है।
....क्योंकि इस समय हमारे सब कर्मों का झुकाव एवं उनके रूप का निर्धारण प्रकृति के द्वारा किया जाता है, और यह प्रकृति यहाँ त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, और समस्त प्राकृत सत्ता में तथा प्रकृतिगत सभी कार्यों में ये तीन गुण विद्यमान रहते हैं, अपने अज्ञान और जड़ता सहित तमस्, अपनी गतिशीलता और क्रिया तथा आवेग, दुःख और विकार से युक्त रजस्, अपने प्रकाश और सुख से युक्त सत्त्व; और फिर समस्त प्राकृत सत्ताओं और कर्मों में इन चीजों का बंधन भी रहता ही है। मान लें कि जीव अपनी अंतःसत्ता में त्रिगुण से ऊपर उठ जाता है फिर भी यह प्रश्न उठता है कि अपनी यंत्र-स्वरूप प्रकृति में वह उनके क्रिया-कलाप, परिणाम तथा बंधन से किस प्रकार मुक्त होता है? क्योंकि, गीता कहती है कि ज्ञानी मनुष्य को भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करना होगा। बाह्य अभिव्यक्ति में गुणों की प्रतिक्रिया को अनुभव तथा सहन करना, पर पीछे अवस्थित साक्षीस्वरूप सचेतन आत्मा में उनसे मुक्त तथा ऊपर रहना ही पर्याप्त नहीं है; क्योंकि स्वतंत्रता और अधीनता का एक द्वैत, तथा जो कुछ हम भीतर हैं और जो कुछ हम बाहर हैं उनके बीच, हमारी आत्मा और हमारी शक्ति के बीच, अपनी सत्ता का जैसा स्वरूप हम जानते हैं तथा हम जो संकल्प एवं कर्म करते हैं उनके बीच एक अंतर्विरोध फिर भी बना रहता है। इसमें मुक्ति कहाँ है, उच्चतर आध्यात्मिक प्रकृति में पूर्ण उत्कर्ष तथा रूपान्तर कहाँ है, सनातन धर्म, भागवत् सत्ता की अनंत पवित्रता एवं शक्ति का निज धर्म कहाँ है? यदि इस देह में रहते हुए यह परिवर्तन साधित नहीं किया जा सकता तब तो यह कहना होगा कि सम्पूर्ण प्रकृति का रूपान्तर करना संभव नहीं और जब तक जीवन का यह मृत्युशील ढाँचा परित्यक्त खोल की भाँति आत्मा से उतरकर अलग नहीं हो जाता तब तक यह इंद्र सुलझे बिना ज्यों-का-त्यों बना रहेगा। पर उस स्थिति में कर्म को यह इन यथोचित नहीं हो सकता या कम-से-कम वह चरम सिद्धान्त तो से ही नहीं सकताः तब तो पूर्ण निस्तब्धता या, कम-से-कम, एक यथासमय पूर्ण निस्तब्धता, उत्तरोत्तर वर्धमान संन्यास और कर्मों का परित्याग ही पूर्णत्व-प्राप्ति के लिए एक सच्चा उपदेश प्रतीत होगा, - जैसे कि मायावादी दावा करता ही है, जो कहता है कि जब तक हम कर्म में बने रहते हैं तब तक गीता का मार्ग निःसंदेह समुचित मार्ग है, परंतु फिर भी समस्त कर्म ही भ्रम है और निस्तब्धता ही सर्वोच्च पथ है। इस भाव से कर्म करना उत्तम अवश्य है पर कर्मत्याग, निवृत्ति एवं पूर्ण निस्तब्धता तक पहुँचने के एक सोपान के रूप में ही।
यही वह कठिनाई है जिसका उत्तर गीता को अभी देना है ताकि वह ईश्वरान्वेषक के लिए कर्मों का औचित्य सिद्ध कर सके....।।
इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि केवल आत्मपरक सत्ता ही नहीं अपितु वस्तुपरक या बाहरी सत्ता भी गुणों की क्रिया से मुक्त हो सकती है। इसके लिए गीता कहती है कि केवल भगवान् की भक्ति के द्वारा ही ऐसा किया जाना संभव है। परंतु गीता ने यहाँ इस विषय को विस्तृतता से उठाकर इसका जिस प्रत्यक्ष रूप में समाधान किया है वैसा उसने पहले नहीं किया था। इस समाधान में गीता साथ ही साथ दो तरीके की प्रकृतियों के लोगों के बीच भेद करती है, एक हैं दैवी प्रकृति से युक्त लोग और दूसरे हैं आसुरी प्रकृति से युक्त लोग। इनमें जो मूलतः दैवी प्रकृति के लोग हैं वे ही भगवान् की ओर जा सकते हैं, दूसरे नहीं।
प्रश्न : देव और असुर तो दोनों भगवान् की ही देन हैं, तब फिर केवल दैवी प्रकृति के लोग ही भगवान् की ओर क्यों जा सकते हैं?
उत्तर : देव और असुर पराप्रकृति के द्वारा सृष्ट किये जाते हैं। जब संसार की अभिव्यक्ति होती है और उच्चतर लोकों से होते हुए निम्नतर लोकों का निर्माण होता है तब निवर्तन की प्रक्रिया में असुर सहायक होते हैं परंतु चेतना जब निश्चेतन स्तरों से क्रमविकास की गति का अनुसरण कर अपने मूलस्रोत तक पुनः आरोहण करती है तब देवता उस गति में सहायक होते हैं और असुर इस आरोहण में बाधक होते हैं। इसलिए हमारे पुराणों आदि में देवताओं को निवृत्तिपरक माना जाता है और असुरों को प्रवृत्तिपरक। इसलिए निवर्तन की प्रक्रिया में निवृत्ति भाव सहायक नहीं होता उसमें तो प्रवृत्ति आवश्यक है। इसीलिए निवर्तन में असुर सहायक होते हैं। कर्म करने का अर्थ प्रकृति के तीन गुणों के अधीन होना है; उसकी क्रिया की इन अवस्थाओं के ऊपर उठने का अर्थ आत्मा में नीरव होकर स्थित रहना है। ईश्वर, पुरुषोत्तम, जो प्रकृति के सब कार्यों और क्रियाओं के स्वामी हैं तथा जो अपने दिव्य संकल्प के द्वारा उन सबका निर्देशन और निर्धारण करते हैं, निःसंदेह गुणों की इस यांत्रिक क्रिया से परे हैं; वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित या आबद्ध नहीं होते; परन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे सदा इन्हीं के द्वारा कार्य करते हैं, सदा स्वभाव की शक्ति से तथा गुणों के मनोवैज्ञानिक यंत्र के द्वारा ही गठन करते हैं। ये प्रकृति के तीन मूलभूत गुण हैं, यहाँ हमारे अन्दर जो कार्यवाहिका प्रकृति-शक्ति गठित हो रही है उसकी ये आवश्यक क्रियाएँ हैं, और स्वयं जीव भी इस प्रकृति के अन्दर भगवान् का एक अंश मात्र है। यदि मुक्त व्यक्ति मुक्ति के बाद भी कर्म करता रहता है, कर्म-प्रपंच में विचरण करता है, तो वह प्रकृति के अन्दर रहता हुआ तथा उसके गुणों के द्वारा सीमाबद्ध एवं उनकी प्रतिक्रियाओं के अधीन होकर ही कर्म कर सकता तथा विचरण कर सकता है, और जब तक उसकी सत्ता का प्राकृत भाग बना रहता है तब तक वह भगवान् की मुक्तावस्था में कर्म नहीं कर सकता। परन्तु गीता ने इससे ठीक विपरीत बात कही है, वह यह कि मुक्त योगी गुणों की प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है और वह चाहे जो भी कर्म करे, चाहे जिस प्रकार भी रहे, पर वह सदा ईश्वर में ही, उनके स्वातंत्र्य और अमृतत्व की शक्ति में ही, परमोच्च शाश्वत अनंत के विधान में ही निवास करता है, उसी में गति तथा कर्म करता है, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक परस्पर विरोध एवं गतिरोध है।
छठे अध्याय के इकतीसवें श्लोक में भी गीता ने स्पष्टतः कहा कि 'जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर समस्त भूतों में मुझसे प्रेम करता है वह योगी चाहे जिस प्रकार रहे और कर्म करे मुझ में ही रहता और कर्म करता है।' अतः जो योगी भगवान् में ही रहता और कर्म करता है उसके ऊपर कर्मबंधन लागू नहीं होते। अलग-अलग स्थानों पर गीता बराबर हो इस ओर संकेत करती है कि जब साधक भगवान् में ही निवास करता है तब वह कर्मबंधन और गुणों से ऊपर रहता है। अतः इस सारे पूरा प्रकाश डाला जाना आवश्यक है। विषय पर
"जब व्यक्ति भागवत् चेतना में निवास करता है तब बाहरी दृष्टि को तो उसके कर्म गुणों के अधीन प्रतीत हो सकते हैं, क्योंकि बाहरी दो को तो केवल उस कर्म की प्रक्रिया गोचर होती है उसके पीछे की किया दिखाई नहीं देती, परंतु वास्तव में उस पर किसी प्रकार के कोई गुण और कर्मों के फल या परिणाम लागू नहीं होते। श्रीमाताजी के कार्य, या फिर भगवान् श्रीकृष्ण की क्रियाएँ भी किसी सामान्य दृष्टि को गुणों के अधीन प्रतीत हो सकती है, परंतु वास्तव में तो वह भागवत् क्रिया होती है जो किसी भी बाहरी प्रक्रिया से बँधी नहीं होती और न ही उस पर गुण लागू होते हैं क्योंकि वह किसी कामना या निजी हेतु से नहीं अपितु भागवत् संकल्प की अभिव्यक्ति के लिए कार्य करती है। अन्यथा मुक्त व्यक्ति भी गुणों के अधीन होकर ही कर्म में प्रवृत्त हुआ नजर आता है।
परन्तु ऐसा तभी दिखायी देता है जब हम विश्लेषक मन के कठोर तार्किक विरोधों के साथ गाँठ बाँध लेते हैं, तब नहीं जब हम आत्मा के स्वरूप, तथा प्रकृति के अन्दर विद्यमान अध्यात्म-सत्ता पर मुक्त एवं सूक्ष्म रूप से दृष्टिपात करते हैं। जो शक्ति जगत् को चला रही है वह वास्तव में प्रकृति के गुण नहीं हैं, - ये गुण तो हमारी सामान्य प्रकृति का केवल निम्नतर पहलू हैं, उसका एक यंत्र मात्र हैं। वास्तविक चालक-शक्ति तो एक आध्यात्मिक भगवत्संकल्प है जो वर्तमान में इन निम्न अवस्थाओं का प्रयोग कर रहा है, पर जो स्वयं मानवीय संकल्प की भाँति गुणों के द्वारा सीमाबद्ध एवं नियंत्रित नहीं होता, उनका यंत्र नहीं बन जाता। निःसंदेह, क्योंकि ये गुण अपनी क्रिया में इतने सार्वभौमिक हैं, इनका मूल परमात्मा की शक्ति के भीतर निहित किसी तत्त्व में ही होना चाहिए; दिव्य संकल्प-बल में ऐसी शक्तियाँ अवश्य होनी चाहिए जिनसे प्रकृति के ये गुण उद्भूत होते हैं। क्योंकि, निम्नतर सामान्य प्रकृति में सभी कुछ पुरुषोत्तम की सत्ता की उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति से हो निःसृत होता है, मत्तः प्रवर्तते; वह बिना किसी आध्यात्मिक मूल कारण के सर्वथा किसी नवीन वस्तु के रूप में उद्भुत नहीं हो जाता। आत्मा की मूल शक्ति में कोई ऐसी चीज अवश्य है जिससे हमारी प्रकृति का सात्त्विक प्रकाश एवं सुख उसकी राजसिक गति तथा तामसिक जड़ता निःसृत हुई हैं और जिसके ये अपूर्ण या विकृत रूप हैं। किन्तु एक बईत जब हम इन रूपों की अपूर्णता एवं विकृति, जिसके अन्दर हम निवाक करते हैं. हे परे इनके स्रोतों के विशुद्ध रूप तक पहुँचते हैं तो हम पाते हैं कि, ज्यों ही हम आत्मा के अन्दर निवास करने लगते हैं त्यों ही, ये गतियाँ एक सर्वथा भिन्न रूप धारण कर लेती हैं। सत्ता और कर्म तथा इन दोनों की त्रिगुणात्मक अवस्थाएँ अपने वर्तमान सीमित रूप से सर्वथा भिन्न और कहीं अधिक उच्चतर वस्तुएँ बन जाती हैं।
इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जब व्यक्ति कोई नाटक प्रस्तुत कर रहा होता है और उसे पूरी कथावस्तु का पता होता है तब वह अपने भाग को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाता है और आवश्यक सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करते हुए भी स्वयं भीतर से जानता है कि यह केवल नाटक है और इससे वह विचलित नहीं होता। परंतु दर्शक को तो उसके भिन्न-भिन्न भावों की प्रतीति होती है जबकि वास्तव में कलाकार की अविचल मानसिक स्थिति उसे गोचर नहीं होती। इसी प्रकार जो भगवान् के संकल्प की ही अभिव्यक्ति करते हैं वे बाहर से तो त्रिगुणात्मक प्रक्रिया के द्वारा ही काम करते प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में वे उन गुणों से लिप्त नहीं होते इसलिए उनकी क्रिया त्रिगुणात्मिका नहीं होती। दर्शक को देखने में प्रतीत हो सकता है कि कलाकार बड़े ही क्रोध में है, जबकि भीतर से वह कलाकार अपने भाग को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके बड़ी संतुष्टि महसूस कर रहा हो सकता है। साथ ही, नाटक का उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा एक संदेश दिया जाए और उसे इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दर्शक उस संदेश को सहज रूप से ग्रहण कर सकें। उसी के अनुरूप संवाद, मंच, साज-सज्जा आदि की व्यवस्था की जाती है ताकि उस नाटक का संदेश दर्शक तक भली-भाँति पहुँच जाए और उस पर उसका गहरा प्रभाव पड़ सके। इसी प्रकार भागवत् कार्य करते समय भी व्यक्ति का उद्देश्य केवल यह होता है कि किस प्रकार प्रभु का कार्य सर्वोत्तम ढंग से किया जाए और उसके लिए वह जब, जहाँ और जैसा आवश्यक होता है वैसा ही व्यवहार करता है। इसलिए वह जो भी भाव आवश्यक होता है वही अभिव्यक्त कर देता है। यदि क्रोध 1 की आवश्यकता हो तो वह क्रोध करने से नहीं हिचकिचाता, यदि युद्ध, संहार आदि घोर कर्म करने हों तो उनसे भी नहीं चूकता। इसीलिए बाहरी दृष्टिकोण से तो ये सभी तामसिक या राजसिक कार्य प्रतीत हो सकते हैं परंतु दिव्य कर्मी की चेतना में तो ये सभी कर्म केवल भागवत् संकल्प की अभिव्यक्ति होने के कारण त्रिगुणों की क्रिया से परे रहते हैं।
जब व्यक्ति परमात्मा की चेतना के अधिकाधिक समीप जाने लगता है तब उसे भीतर से आभास प्राप्त होने लगता है कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। तब उसे इससे सरोकार नहीं रहता कि यह तामसिक कार्य है या राजसिक या सात्त्विक। उसकी चेतना में इन सभी चीजों का कोई स्थान नहीं रहता क्योंकि वह तो सर्वथा एक भिन्न चेतना में निवास करता है। बाहरी रूप से तो श्रीमाताजी भी किसी पर क्रोष कर देती थीं, और किसी के ऊपर क्रोध करने का बाहरी कारण होते हुए भी अनुग्रह दिखाती थीं, किसी को राजसी सुविधाएँ प्रदान करती थीं तो किसी को केवल मूलभूत सुविधाएँ ही प्रदान करती थीं। इसलिए बाहरी दृष्टिकोण से उनके व्यवहार के द्वारा कोई भी कह सकता था कि उनको क्रियाएँ त्रिगुणात्मिका थीं। परंतु वे सदा ही आत्मा के दृष्टिकोण से जैसा जिसके साथ आवश्यक होता था वैसा ही उसके साथ व्यवहार करती थीं। इसी कारण प्रत्येक के साथ व्यवहार में अंतर होते हुए भी प्रत्येक भली-भाँति जानता था कि श्रीमाँ उससे अतिशय प्रेम रखती हैं और उसके लिए जो आवश्यक है वही करती हैं।
श्रीअरविन्द के अनुसार पराप्रकृति के अंदर अपने सच्चे स्वरूप में स्थित समता, तपस् और ज्योति ही निम्न प्रकृति में भ्रष्ट होकर तमस्, रजस् और सत्त्व बन जाते हैं। इसलिए ये तो केवल भ्रष्ट रूप हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। दिव्य कर्मी वास्तव में समता, तपस् और ज्योति के अनुसार ही काम करता है परंतु निम्न प्रकृति के वशीभूत होने के कारण हम उन्हें उनके भ्रष्ट रूपों से समझ बैठते हैं।
इसे देखने का एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि वास्तव में इस जगत् में जगज्जननी के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है। जब भगवान् की पराशक्ति जगज्जननी कर्ती होती है तब उसे प्रकृति कहते हैं और जब वह क्रिया का साक्षित्व करती है तब उसे पुरुष कह देते हैं। अतः अभिव्यक्ति में पराप्रकृति ही हमारी आत्मा बनती है, वही प्रकृति बनती है, और वही पुरुष बनती है। सारी क्रीड़ा उसी की है। और केवल एक मानसिक उपकरण के माध्यम से देखने के कारण ही हमें यह क्रीड़ा त्रिगुणमयी प्रतीत होती है जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तो वैसा ही है जैसे कि रंगीन चश्मे के द्वारा हमें सारा जगत् उसी रंग का नजर आने लगता है जबकि वह वैसा होता नहीं है। अतः जब हम अपनी मानसिक चेतना के माध्यम से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं तब हमें वे त्रिगुणमयी प्रतीत होती हैं। यहाँ तक कि जो उच्चतर गुण हैं वे भी केवल देखने का तरीका मात्र ही हैं क्योंकि वास्तव में तो सभी कुछ केवल जगदम्बा के संकल्प के द्वारा ही संसिद्ध होता है और वह किन्हीं भी गुणों या प्रक्रिया आदि से बाध्य नहीं है। निम्न प्रकृति में गुणों का आभास अज्ञान की उपज है। जब अज्ञान मिट जाता है तब वह गुणों का आभास भी स्वयमेव ही लुप्त हो जाता है। जैसे-जैसे चेतना के स्तर में बदलाव आता है वैसे-वैसे ही यह जगत्-दृश्य बदलता जाता है। जैसा संसार मनुष्यों को नजर आता है वैसा पशुओं को नहीं आता। और जैसा जगत् देवताओं को गोचर होता है वैसा मनुष्यों को गोचर नहीं होता। इसलिए चेतना के स्तर पर निर्भर करता है कि जगत् की प्रतीति कैसी होगी। इसीलिए गीता कहती है कि जो भगवान् की भक्ति करता है वह तीनों गुणों से परे चला जाता है। यह तो स्वाभाविक ही है कि जब व्यक्ति भगवान् की भक्ति करता है तब अधिकाधिक वह भगवान् की चेतना में निवास करने लगता है और चूँकि भगवान् की चेतना में गुणों का कोई अस्तित्व ही नहीं है इसीलिए वह साधक भी तीनों गुणों से परे चला जाता है।
समस्त द्वंद्व और संघर्ष से युक्त जगत् की इस विक्षुब्ध गति के पीछे क्या चीज है? वह कौन-सी चीज है जो मन को छूते ही, मानसिक रूप धारण करते ही कामना, चेष्टा, श्रम, भ्रांत संकल्प, पाप और दुःख-दर्द की प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती है? वह गति में प्रवृत्त आत्मा का संकल्प है, कर्मरत विराट् भगवत्-संकल्प है जो इन चीजों से प्रभावित नहीं होता; वह मुक्त एवं अनंत चेतन परमेश्वर की एक शक्ति' है जिसमें कोई कामना नहीं, क्योंकि वह विश्व की समस्त संपदा की स्वामिनी है और अपनी गति के सहज-स्फूर्त आनन्द की भोक्त्री है। किसी प्रकार के प्रयत्न तथा श्रम से क्लांत न होती हुई वह अपने साधनों तथा उद्देश्यों के निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करती है; संकल्प की किसी भी त्रुटि के कारण पथ भ्रष्ट न होती हुई वह आत्मा और वस्तुओं के एक ऐसे ज्ञान को धारण करती है जो उसके प्रभुत्व और आनंद का मूल स्रोत हैः किसी भी दुःख, पाप या वेदना से पराभूत हुए बिना वह अपनी सत्ता के और शक्ति के आनंद और पवित्रता से युक्त है। जो जीव ईश्वर में निवास करता है वह इस आध्यात्मिक संकल्प के द्वारा कार्य करता है, न कि बंधनग्रस्त मन के सामान्य संकल्प के द्वाराः उसकी समस्त क्रिया-प्रवृत्ति इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा होती है, प्रकृति के रजोगुण के द्वारा नहीं, ठीक इस कारण क्योंकि वह अब और उस निम्नतर गति, जिससे यह विकृति सम्बद्ध है, में निवास नहीं करता, अपितु दिव्य प्रकृति में गति के विशुद्ध और पूर्ण मर्म पर पहुँच गया होता है।
गुणों का संघर्ष तो निम्न प्रकृति की अपूर्णता में (भगवान् की दिख प्रकृति का) एक प्रकार का अपूर्ण प्रतिरूप मात्र है; तीनों गुण जिन शक्तियों के द्योतक हैं वे भगवान् की तीन मूल शक्तियाँ हैं जो न केवल एक पूर्ण शान्तिमय सन्तुलन में ही स्थित हैं अपितु दिव्य कर्म के एक पूर्ण सामंजस्य में एकीभूत भी हैं। आध्यात्मिक सत्ता में तमस् दिव्य शांति बन जाता है, जो कि कोई जड़ता या कार्य करने की अक्षमता नहीं होती अपितु एक पूर्ण शक्लि होती है जो अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य को अपने अन्दर धारण किये रहती है और अत्यन्त विशाल एवं बृहत् कर्म तक को भी नियन्त्रित करने तथा शान्ति के नियम के अधीन बनाने में समर्थ होती है: रजस् आत्मा की आत्म-सिद्धिकारी, प्रवर्तक विशुद्ध संकल्पशक्ति बन जाता है, जो कि कामना, प्रयत्न एवं आयासपूर्ण आवेश नहीं रहती अपितु सत्ता की वही पूर्ण शक्ति होती है जो अनन्त, अक्षुब्ध एवं आनन्दपूर्ण कर्म करने में समर्थ है। सत्त्व एक विकृत मानसिक प्रकाश न रहकर दिव्य सत्ता की वह स्वयंभू ज्योति बन जाता है जो सत्ता की पूर्ण शक्ति की सारभूत अथवा आत्मा है और दिव्य शान्ति तथा कर्मसम्बन्धी दिव्य संकल्पशक्ति दोनों के एकत्वमय स्वरूप को आलोकित करती है।.... वह ज्योति प्रकाशपूर्ण अध्यात्म-संकल्प से परिपूर्ण है और उसके ज्ञान तथा उसके कर्म में कोई खाई या विषमता नहीं है। वह आनंद हमारा क्षीणतर मानसिक सुख नहीं है, अपितु गंभीर, तीव्र, प्रगाढ़, स्वयंसत् आनंद है; हमारी सत्ता जो कुछ भी करती है, जिस भी वस्तु की परिकल्पना एवं सृष्टि करती है उस सब में वह आनन्द व्याप्त रहता है, वह एक स्थिर दिव्य आनंद है। मुक्त जीव इस ज्योति और आनन्द में अधिकाधिक गंभीर रूप से सहभागिता करता है, जितना ही अधिक पूर्ण रूप में वह इसके अन्दर वर्धित होता है, उतना ही अधिक समग्र रूप में वह अपने-आप को भगवान् के साथ युक्त कर देता है। जहाँ निम्न प्रकृति के गुणों में रहते हुए, आवश्यक रूप से, एक असंतुलन बना रहता है, उनकी मात्रा में अस्थिर रूप से बदलाव आता रहता है, तथा आधिपत्य जमाने के लिए सतत् संघर्ष रहता है;
-------------------------------
'तपस्, चित्-शक्ति
वहीं इसके विपरीत, अध्यात्म-सत्ता की महत्तर ज्योति एवं आनन्द, स्थिरता और गति-संकल्प एक-दूसरे का बहिष्कार नहीं करते, परस्पर संघर्ष नहीं करते, यहाँ तक कि ये एक संतुलित ही नहीं रहते वरन् इनमें से प्रत्येक शेष दो का एक अंग है अब अपनी पूर्णता में ये सब एक एवं अविभाज्य हैं। हमारा मन जब भगवान् औरसकट पहुँचता है तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वह इनमें से एक का कान कर दूसरे में प्रवेश कर रहा है, उदाहरणार्थ, ऐसा दिखायी दे सकता है कि वह कर्म की प्रवृत्ति को त्यागकर शांति उपलब्ध करना चाहता है, पर इसका कारण यह है कि पहले-पहल हम अपने मन की चुनाव करने की वृत्ति के द्वारा ही उनकी ओर अग्रसर होते हैं। बाद में जब हम आध्यात्मिक मन से भी ऊपर उठने में समर्थ हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि इन दिव्य शक्तियों में से प्रत्येक के अन्दर शेष सब भी विद्यमान हैं और तब हम इस प्रारम्भिक भूल से छुटकारा पा सकते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव के प्रकृति के गुणों की सामान्य हीन क्रिया के अधीनस्थ हुए बिना भी कर्म संभव है। वह क्रिया मन-प्राण-शरीर रूपी जिस सीमित साँचे में हम ढले हैं उसी के ऊपर निर्भर करती है; यह एक विकृति है, एक अक्षमता, एक दोषपूर्ण या हीन मूल्य है जिसे जड़भौतिक में बद्ध मन और प्राण हम पर लादते हैं। जब हम आत्मा में अभिवर्द्धित होते हैं तो प्रकृति के इस धर्म या निम्न विधान का स्थान आत्मा का अमर धर्म ले लेता है; तब मुक्त अमर कर्म, दिव्य असीम ज्ञान, परात्पर शक्ति और अपार विश्रांति का अनुभव हमें प्राप्त होता है। पर फिर यह अवस्थांतर या संक्रमण संबंधी प्रश्न शेष रह जाता है; क्योंकि मध्यवर्ती अवस्थाओं, प्रगति के क्रमों का रहना आवश्यक है, क्योंकि इस संसार में ईश्वर की कार्यपरंपरा में कोई भी चीज बिना किसी प्रक्रिया या आधार के किसी आकस्मिक क्रिया के द्वारा नहीं होती। जिस चीज की हम खोज कर रहे हैं वह हमारे अपने ही अन्दर है, परंतु हमें अपनी प्रकृति के निम्नतर रूपों में से उसे विकसित करने के लिए उसे क्रियात्मक रूप में अभ्यास में लाना होगा। अतएव स्वयं गुणों की क्रिया में भी किसी ऐसे उपाय या सुविधाजनक साधन एवं आधार-बिन्दु का होना आवश्यक है जिसके द्वारा हम यह रूपांतर साधित कर सकें। गीता इस उपाय को पाती है सत्त्वगुण के पूर्ण विकास में जब तक कि वह अपने शक्तियारक विस्तार में एक ऐसे स्तर पर नहीं पहुँच जाता जहाँ से वह अपने को अतिकिलो कर सके तथा अपने उद्गम में विलीन हो सके। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि सत्त्व प्रकाश और सुख (प्रसन्नता) की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो शांति और ज्ञान ले आती है, और अपनी उच्चतम स्थिति में यह, जिस आध्यात्मिक ज्योति एवं आनंद से उत्पन्न हुआ है, उसे कुछ-न-कुछ प्रतिभासित कर सकता है, यहाँ तक कि उसके साथ लगभग एक मानसिक तादात्म्य प्राप्त कर सकता है। शेष दो गुण प्रकृति की सत्त्वगुण की शक्ति के हस्तक्षेप के बिना इस प्रकार का रूपांतर लाभ नहीं कर सकते, अर्थात् रजस् दिव्य क्रियाशील संकल्प में अथवा तमस् दिव्य शम और विश्रांति में रूपांतरित नहीं हो सकते।.... सात्त्विक गुण परा और अपरा प्रकृति के बीच प्रथम मध्यस्थ है। सत्त्वगुण को तब तक विकसित करना जब तक कि वह आध्यात्मिक ज्योति, शान्ति और प्रसन्नता या सुख से परिपूर्ण नहीं हो जाता, यही प्रकृति की इस प्रारम्भिक साधना की पहली शर्त है।
जब तक हमारी प्रकृति अपने निम्न स्पंदनों में ही रमी रहती है तब तक उसे इन गुणों की ही प्रतीति होती रहेगी। इसके लिए तो उच्चतर पराप्रकृति को ही आकर इसकी सहायता करनी होगी और इस निम्न प्रकृति का रूपांतर करना होगा। तभी गुणों की इस क्रिया का अंत हो सकता है। अन्यथा तो व्यक्ति जब तक समाधि अवस्था में रहता है तब तक तो उसके आत्मपरक भागों को त्रिगुणों से मुक्ति मिल जाती है परंतु ज्यों ही वह इस निम्न प्रकृति में आता है त्यों ही पुनः उसी प्रपंच में बँध जाता है। इसलिए इस निम्न प्रकृति में भी व्यक्ति सफल रूप से गुणों से परे रहते हुए क्रिया कर पाए, उसके लिए रूपांतर की आवश्यकता है। और रूपांतर तभी साधित हो सकता है जब हम श्रीमाताजी की शक्ति को अपनी प्रकृति के द्वारा मुक्त रूप से क्रिया करने का मौका प्रदान करते हैं। यही समर्पण है।
---------------------------------------------
* उच्चतम प्रकृति की क्रिया के ये परम आध्यात्मिक एवं अतिमानसिक रूप निम्न प्रकृति के तीन गुणों के अनुरूप हैं; इनका जो वर्णन यहाँ किया गया है वह गीता से नहीं लिया गया है अपितु वह आध्यात्मिक अनुभूति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। गीता उच्चतम प्रकृति की क्रिया का, रहस्यम् उत्तमम्, का किंचित् भी वर्णन नहीं करती, वह इसे जिज्ञासु पर छोड़ देती है ताकि वह स्वयं अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा इसे उपलब्ध करे। वह केवल उच्च सात्विक स्वभाव और कर्मवाली प्रकृति का निर्देश भर कर देती है जिसके द्वारा यह परम रहस्य प्राप्त किया जा सकता है, और साथ ही वह सत्व के भी ऊपर उठने तथा तीनों गुणों को पार करने के लिए आग्रह करती है।
• यह बात आत्म-विजय, पुरुषार्थ और साधना के द्वारा आरोहणशील हमारी प्रकृति के दृष्टिकोण से है। पर इसके साथ ही हमारी सत्ता का रूपांतर करने के लिए इसके अंदर दिव्य ज्योति, उपस्थिति और शक्ति का अवतरित होना तथा अधिकाधिक हस्तक्षेप करना भी आवश्यक है; अन्यथा सिद्धि के चरम बिंदु पर तथा उसके परे रूपांतर साधित नहीं हो सकता। इसी कारण साधना की अंतिम गति के रूप में पूर्ण आत्म-समर्पण की आवश्यकता होती है।
इस हम देखेंगे कि गीता के शेष अध्यायों का संपूर्ण अभिप्राय यही है। परंतु प्रबोधनकारी प्रक्रिया की विवेचना करने से पहले इसकी भूमिका के रूप मैं वह दो प्रकार की सत्ताओं, देव और असुर, के बीच भेद दिखलाती है: क्योंकि देव एक उच्च आत्म-रूपांतरकारी सात्त्विक क्रिया में समर्थ है, असुर असमर्थ। हमें यह देखना होगा कि इस भूमिका का उद्देश्य तथा इस भेद की यथार्थ उपयोगिता क्या है। सभी मनुष्यों की सामान्य प्रकृति एक-सी है; वह तीन गुणों का मिश्रण होती है; अतः, ऐसा प्रतीत होगा कि सत्त्वगुण को विकसित और परिपुष्ट करने तथा उसे दिव्य रूपांतर की ऊँचाइयों की ओर उन्मुख कर देने की क्षमता सबके अंदर है। चूँकि हमारी सामान्य प्रवृत्ति वास्तव में अपनी बुद्धि और संकल्प को अपने राजसिक या तामसिक अहंभाव का दास बनाने की तथा अपनी बेचैन एवं असंतुलित गतिशील कामना या आत्म-विलासी अथवा भोग में आसक्त अकर्मण्यता और निष्क्रिय जड़ता के सेवक बना देने की ओर होती है, हम मान सकते हैं कि यह केवल हमारी अविकसित आध्यात्मिक सत्ता की एक अस्थायी प्रवृत्ति एवं इसके अपूर्ण विकास की अपरिपक्व अवस्था ही हो सकती है, और यह तब अवश्य दूर हो जाएगी जब हमारी चेतना आध्यात्मिक श्रेणी में ऊँची उठ जाएगी। परंतु वास्तव में हम देखते हैं कि मनुष्य, कम-से-कम एक स्तर-विशेष से ऊपर के मनुष्य, अधिकांशतः दो श्रेणियों के अंदर आते हैं, एक तो वे लोग जिनमें ज्ञान, आत्म-संयम, परोपकार तथा पूर्णता की ओर प्रवृत्ति रखने वाली सात्त्विक प्रकृति की प्रबल शक्ति होती है और दूसरे वे जिनमें राजसिक प्रकृति की प्रबल शक्ति होती है जो अहंकारमय महत्ता, कामना-पूर्ति की ओर तथा अपने निजी दृढ़ संकल्प एवं व्यक्तित्व में लिप्तता की ओर मुड़ी रहती है जिसे (इस दृढ़ संकल्प और व्यक्तित्व को) वे भगवान् की सेवा के लिए नहीं, अपितु अपने अभिमान, यश और सुख के लिए जगत् पर लादना चाहते हैं।
----------------------------
* अज्ञान का अर्थ है अविद्या, पृथक्कारी चेतना और उससे निकलने वाले अहंकारमय मन और प्राण तथा वह सब जो पृथक्कारी चेतना तथा अहंकारमय मन और प्राण के स्वभाव के अनुरूप ही हो... मिथ्यात्व, दूसरी ओर, यह अविद्या नहीं है, अपितु उसका एक घोर परिणाम है। । यह एक आसुरिक शक्ति के द्वारा सृष्ट होता है जो इस सृष्टि में हस्तक्षेप करती है और जो कि केवल सत्य से ही विच्छिन्न नहीं है जिसके कारण कि वह ज्ञान में सीमित और भ्रांति की ओर खुली है, अपितु सत्य के विरुद्ध विद्रोह करती है या सत्य को केवल विकृत करने के लिये ही उसे अधिकृत करने की अभ्यासी होती है...
ये वे शक्तियाँ और सत्ताएँ हैं जो अज्ञान के जगत् में अपने रचे मिथ्यात्वों को बनावे रखने में और उन्हें ऐसे सत्य के रूप में सामने रखने में रुचि रखती हैं जिनका अनुसरण मनुष्यों को आवश्यक रूप से करना ही होगा। भारत में उन्हें असुर, राक्षस, पिशाच (क्रमशः मानसीकृत प्राण, मध्य प्राण और निम्नतर प्राण के लोकों की सत्ताएँ) की संज्ञा दी गई है जो कि देवताओं, अर्थात् ज्योति की शक्तियों के विरुद्ध हैं।
यदि कोई विरोधी शक्तियाँ नहीं होती, और फिर भी उनके बिना ही क्रमविकासमय जगत् होता, तो अज्ञान तो तब भी हो सकता था परंतु अज्ञान में कोई विकृति या भ्रष्टता नहीं होती। सभी कुछ एक आंशिक सत्य होता जो अपूर्ण उपकरणों के द्वारा कार्य कर रहा होता परंतु एक विकासशील अभिव्यक्ति की इस या उस अवस्था के भले-से-भले प्रयोजनों के लिए कार्य कर रहा होता।
* असुर और राक्षस आदि पृथ्वी की नहीं अपितु अति-भौतिक जगतों से संबद्ध सताएँ हैं: परंतु वे पार्थिव जीवन पर क्रिया करती हैं और मानव जीवन और चरित्र और कर्म पर अधिकार जमाने के लिये देवताओं सरती हैं और मानव जीवन और चरित्र हैं जो ज्योति की शक्तियों से संघर्ष करती हैं।
कभी-कभी वे मनुष्यों के द्वारा कार्य करने के लिये उन्हें अधिकृत कर लेती हैं। कभी-कभी मनुष्य-शरीर में जन्म ले लेती हैं। जब जागतिक लोला में उनका उपयोग खत्म हो जाएगा तब वे या तो परिवर्तित हो जाएँगी या बिलक हो जाएँगी या पृथ्वी-लीला में हस्तक्षेप करने का फिर और प्रयत्न नहीं करेंगी।
ये देवों और दानवों या असुरों के मानवीय प्रतिनिधि हैं। यह भेद भारतीय धार्मिक प्रतीकवाद में अत्यंत प्राचीन है।.... हमारे मन की अपेक्षा भौतिक आवरण के पीछे छिपे हुए वस्तुओं के सत्य की ओर अधिक खुले हुए प्राचीन मानव के मन ने मानव-जीवन के पीछे उन महान् वैश्व शक्तियों या सत्ताओं को देखा था मत विश्व-शक्ति की कुछ एक प्रवृत्तियों या कोटियों की, दैवी, आसुरी, सहयो और पैशाची प्रवृत्तियों या कोटियों की प्रतिनिधि हैं; और जो लोग अपने अंदर प्रकृति की इन विशिष्ट प्रवृत्तियों का प्रबल रूप से प्रतिनिधित्व करते थेने स्वयं भी देव, असुर, राक्षस और पिशाच" समझे जाते थे। गीता अपने प्रयोजनों के लिए इस भेद को स्वीकार करती है और इन दो प्रकार की सत्ताओं के विभेद को विशद रूप से विकसित करती है, द्वौ भूतसगौं। वह पहले ही उस प्रकृति का वर्णन कर चुकी है जो आसुरी और राक्षसी है और ईश्वर-ज्ञान, मुक्ति और पूर्णता में बाधा डालती है; अब वह इन चीजों की ओर मुड़ी हुई दैवी के साथ इसकी तुलना करती है।
प्रश्न : क्या श्रीअरविन्द की टीका का यह अभिप्राय है कि जिन लोगों में आत्म-रूपांतरकारी सात्त्विक क्रिया की संभावना है वे दैवी प्रकृति के होते हैं अन्यथा आसुरी प्रकृति के होते हैं?
उत्तर : वास्तव में अधिकांश लोगों में दैवी और आसुरी दोनों ही वृतियों का कुछ मिला-जुला रूप होता है और इसलिए अपने जीवन में वे कोई भी निर्णायक कार्य नहीं कर पाते और एक बड़ा ही सामान्य, निस्तेज, अनुपयोगी प्रकार का जीवन ही जीते हैं। केवल कुछ थोड़े ही हैं जिनमें प्रबल रूप से या तो दैवी प्रकृति का प्रभाव होता है या फिर आसुरी प्रकृति का। ऐसे लोग अपने जीवन में अतिविशाल, महान् या घोर कर्म संसिद्ध करते हैं। पृथ्वी पर जो भी महान् उपलब्धियाँ या अतिविराट् कर्म किये गए हैं वे ऐसे ही लोगों के द्वारा किये गए हैं। हमारे पुराणों आदि में हम ऐसे ही दैवी प्रकृति के व्यक्तियों या फिर आसुरी प्रकृति के व्यक्तियों का वर्णन पाते हैं। देव और असुर दोनों ही अपने-अपने स्तर विशेष पर बँधे होते हैं इसलिए इनमें से कुछ पृथ्वी पर मनुष्यों को प्रभावित कर, उनके साथ संयुक्त होकर, या उन्हें आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने अधिकार में लेकर अपनी अभिव्यक्ति का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी तो वे मानव देह में जन्म भी ग्रहण कर सकते हैं। केवल मानव ही है जो क्रमविकासमय सत्ता है। अतः जो दैवी प्रकृति के संपर्क में हैं या उनसे प्रभावित हैं वे मनुष्य तो आत्म-रूपांतर, आत्म-विकास कर सकते हैं जबकि जो आसुरी प्रकृति के प्रभाव में हैं वे यह विकास नहीं कर सकते। जब आसुरी वृत्ति का प्रभाव होता है तब वह मनुष्य के चैत्य पुरुष को दबाने का, उसे निष्कासित करने का प्रयास करता है। और जब पूर्ण आसुरी प्रभाव होता है, या फिर जन्म ही आसुरी प्रकृति का होता है तब उसमें चैत्य पुरुष नहीं होता, और यदि होता भी है तो वह इतना दब चुका होता है कि बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाता है। हालाँकि यह एक ऐसा विषय है जो अत्यंत जटिल है।
प्रश्न : अज्ञान और मिथ्यात्व के बीच क्या भेद है?
उत्तर : मिथ्यात्व मानसिक चेतना के प्रादुर्भाव के साथ आता है उससे पहले की चेतना के स्तर पर हम मिथ्यात्व नहीं पाते। पशु और वनस्पति जगत् में हम मिथ्यात्व नहीं पाते। श्रीमाताजी तो अपनी एक वार्ता (११ मार्च १९६१) में ऐसे एक काल का वर्णन करती हैं। यह वार्ता इस विषय को बहुत स्पष्ट कर देती है इसलिए हम इसके अंश यहाँ प्रस्तुत करते हैं। श्रीमाताजी से जब यह पूछा गया कि 'क्या यह सच है कि कोई पार्थिव स्वर्ग भी था? मनुष्य को वहाँ से क्यों निकाल दिया गया?' तो इसके उत्तर में श्रीमाँ कहती हैं, "ऐतिहासिक दृष्टिकोण से (मैं यहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कह रही हैं). यदि मैं अपनी स्मृतियों के आधार पर कहूँ, - मैं इसे प्रमाणित तो नहीं कर सकती; वस्तुतः कुछ भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता, और मुझे नहीं लगता कि यथार्थतः कोई ऐतिहासिक प्रमाण है भी, अर्थात्, ऐसा प्रमाण जिसे सुरक्षित रखा गया हो, कम-से-कम ऐसा कोई प्रमाण अभी तक तो मिला नहीं है – किंतु मुझे जो याद है उसके अनुसार, पृथ्वी के इतिहास में निश्चय ही एक ऐसा समय था जब एक प्रकार के पार्थिव स्वर्ग का अस्तित्व था, इस अर्थ में कि वह एक पूर्णतया सामंजस्यपूर्ण और प्राकृतिक जीवन था; अर्थात्, मन की अभिव्यक्ति बिना किसी विकार या विरूपता के प्रकृति की आरोहणकारी गति के साथ तब तक भी पूर्ण सहमति और सामंजस्य में थी। यह स्थूल रूपों में मन की अभिव्यक्ति की पहली अवस्था थी।
यह कितने समय तक रही? यह कहना कठिन है। किंतु मनुष्य के लिये यह एक ऐसा जीवन था जो कुछ-कुछ पशु-जीवन के उत्फुल्लन से मिलता था। मुझे एक ऐसे जीवन की स्मृति है जिसमें शरीर अपने प्राकृतिक वातावरण के पूर्णतः अनुकूल था और जलवायु शरीर को आवश्यकताओं के और शरीर जलवायु की आवश्यकताओं के अनुकूल था। जीवन ठीक वैसे ही पूर्णतया सहज और स्वाभाविक था जैसे कि एक अधिक प्रबुद्ध और सचेतन पशु-जीवन होता है; परंतु इसमें वे कोई भी जटिलताएँ और विकृतियाँ नहीं थीं जिन्हें मन अपने विकासक्रम में बाद में ले आया। मुझे उस जीवन की स्मृति है - मुझे यह स्मरण था और जब मैं समग्र रूप से पृथ्वी के जीवन के प्रति सचेतन हुई तब मैंने इसे फिर से जीवन में भी देखा। किंतु मैं यह नहीं कह सकती कि यह कितने समय रहा और न ही यह कि इसका विस्तार कहाँ तक था। मैं नहीं जानती। मुझे केवल अवस्था या स्थिति का ही स्मरण है, अर्थात्, जड़-प्रकृति कैसी थी, उस समय मानव-रूप और मानव-चेतना कैसी थी और पृथ्वी के अन्य सब तत्त्वों के साथ उसका समन्वय कैसा था - साथ, तथा वनस्पति के जीवन के साथ ऐसा उत्कृष्ट समन्वय। वस्तुओं के - पशु-जीवन के प्रयोग का, वनस्पतियों और फलों के गुणों का, वस्तुतः जो कुछ प्रकृति में बनस्पति-जगत् हमें दे सकता था उस सबका वहाँ एक प्रकार का सहज ज्ञान था। कोई आक्रामकता नहीं, कोई भय नहीं, कोई अंतर्विरोध नहीं, न कोई घर्षण और न ही किसी भी प्रकार की विकृति ही - मन पवित्र, सरल और प्रकाशयुक्त, जटिलतारहित था।
क्रमविकास की प्रगति, उसकी अग्रगति के साथ ही, जब मन ने अपने अंदर, अपने ही लिये, विकसित होना शुरू कर दिया तब ये समस्त जटिलताएँ और विकृतियाँ आरंभ हुईं।...
....मुझे यह स्मृति बार-बार, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में, कई बार प्राप्त हुई है। उसमें ठीक वही दृश्य या प्रतिमूर्तियाँ नहीं थीं, क्योंकि यह कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे मैंने देखा हो, यह तो एक ऐसा जीवन था जो मैंने जिया था। कुछ समय तक, रात-दिन एक प्रकार की समाधि की अवस्था में मैं एक ऐसे जीवन में गई जिसे मैंने जिया था, और मुझमें इस बात की पूरी सचेतनता थी कि यह पृथ्वी पर मानव आकार के प्रस्फुटन की अवस्था थी - उन पहले मानव आकारों की जो भागवत् सत्ता को मूर्तिमंत करने में सक्षम थे। हाँ, ऐसा ही था। पहली बार मैं एक पार्थिव आकार में, एक आकार विशेष में, एक वैयक्तिक आकार में अभिव्यक्त हो सकी थी - किसी 'सामान्य' जीवन में नहीं अपितु एक व्यष्टिगत रूप में - अर्थात्, पहली बार इस जड़-पदार्थ के मानसीकरण के द्वारा, ऊपर की सत्ता और नीचे की सत्ता को संयुक्त किया गया था। मैंने इसे अनेकों बार जिया है, पर सदा ही एक जैसे बाहरी परिवेश में और एक ही जैसी अनुभूति - बिना किसी जटिलता के, बिना किन्हीं समस्याओं के, बिना इन प्रश्नों के ऐसी अद्भुत हर्षपूर्ण सरलता की अनुभूति; वहाँ ऐसी कोई समस्याएँ नहीं थीं, ऐसा कुछ भी नहीं था! था तो बस व्यापक प्रेम और सामंजस्य में जीने का हर्ष - फूल, धातु, पशु : सभी सामंजस्य में थे।
यह तो इसके बहुत समय बाद ही ऐसा हुआ - यह भी एक व्यक्तिगत आभास ही है - बहुत समय बाद, कि चीजें गड़बड़ होने लगीं। कदाचित् इसलिये क्योंकि सामान्य क्रमविकास के लिये कुछ-कुछ मानसिक दृढ़ीकरण आवश्यक था, अनिवार्य हो गया था, जिससे कि वह किसी और चीज तक पहुँचने के लिये तैयार हो जाय। और यहीं जजसा .... उफ्! यह तो किसी गड्ढे में, कुरूपता में, अन्धकार में जा गिरने है; इसके बाद सभी कुछ इतना काला, इतना भद्दा, इतना कठिन, बदलता पीड़ादायक हो गया, यह सचमुच, हाँ, सचमुच ही पतन का आभास देता है।" (CWM 10, 88-91)
श्रीमाताजी के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी पर ऐसे समय रहे हैं जब पूर्ण सामंजस्य स्थापित था और चीजों में वह कुरूपता और विकृति नहीं थी जो मन के विकास के साथ हमें देखने को मिलती और श्रीअरविन्द भी अपने सावित्री महाकाव्य के एक संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कुछ-कुछ इस प्रकार प्रकाशित करते हुए कहते हैं कि, “यदि कोई प्रतिरोध न हो तो आवश्यक नहीं कि अचेतन से होने वाला क्रमविकास पीड़ादायक हो; यह सोच समझकर धीरे-धीरे चलने वाला और भगवान् का सुंदर प्रस्फुटन हो सकता था। किसी को भी यह देखने में समर्थ होना चाहिये कि बाहरी प्रकृति कितनी सुंदर हो सकती है और सामान्यतः होती ही है, यद्यपि यह स्वयं ऊपर से देखने में 'निश्चेतन' है। तब आंतरिक प्रकृति में होनेवाले चेतना के विकास के साथ इतना अधिक भद्दापन और बुराई क्यों जुड़ गईं जो बाहरी सृष्टि के सौंदर्य को बिगाड़ देती है? अज्ञान से उत्पन्न होने वाली विकृति के कारण, जो कि 'जीवन' के साथ आई और 'मन' में अभिवर्धित हो गई - वही है मिथ्यात्व, वह अशुभ जो निश्चेतना की पूर्ण निद्रा के कारण उत्पन्न हुआ और यह निद्रा ही इसके कार्य को उस गुह्य चेतन पुरुष की प्रकाशपूर्णता से दूर करती है जो सदा-सर्वदा इसके भीतर विद्यमान रहता है। परंतु ऐसा होना आवश्यक नहीं था, यदि इसके लिए परात्पर प्रभु की सर्वअतिक्रमी संकल्पशक्ति न होती और इसका तात्पर्य यह है कि निश्चेतना और अज्ञान के द्वारा विकृति की संभावना अभिव्यक्त होनी चाहिये ताकि अभिव्यक्ति के अवसर के कारण उन्हें समाप्त किया जा सके, चूँकि सभी संभावना को कहीं न कहीं तो अभिव्यक्त होना ही है : अतः एक बार जब यह समाप्त कर दी जाती है तो जड़तत्त्व में 'भागवत् अभिव्यक्ति' अन्यथा जैसी हुई होती उससे महत्तर होगी क्योंकि इस कठिन सृष्टि के अंदर जितनी भी संभावनाएँ छिपी पड़ी हैं वे सब की सब एक साथ संयुक्त हो जाएँगी - उनमें से कोई-कोई ही नहीं जैसा कि किसी अधिक आसान और कम श्रमसाध्य सृष्टि में स्वभावतया घटित होता।" (CWSA 27, p. 304)
इस प्रकार श्रीअरविन्द भी इसकी पुष्टि करते हैं कि किसी समय विशेष पर भागवत् संकल्प ने ऐसी संभावना देखी और मिथ्यात्व को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया ताकि इस सृष्टि का कुल परिणाम अधिक समृद्ध हो सके और अभिव्यक्ति प्रदान करके इन अंधतर शक्तियों को आमूल नष्ट किया जा सके। यदि इन्हें अवसर न दिया जाता तो हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रकृति में अज्ञान तो होता परंतु मिथ्यात्व होना आवश्यक नहीं था। तब विकास अज्ञान से ज्ञान की ओर, सौंदर्य से अधिक सौंदर्य की ओर होता। प्रकृति में हम अज्ञान तो देखते हैं परंतु मिथ्यात्व नहीं। यहाँ तक की भीषण प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे कि आँधी-तूफान, चक्रवात, ज्वालामुखी आदि भी केवल मानव चेतना के लिए तो अधिक ग्राह्य नहीं हैं परंतु अपने आप में उनमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। पशु जगत् में हम जीवन के लिए संघर्ष अवश्य देखते हैं परंतु मिथ्यात्व नहीं देखते। मिथ्यात्व तो तब होता है जब हम किसी गलत चीज को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वनस्पति और पशु जगत् में ऐसा कोई प्रयास दिखाई नहीं देता। यदि मिथ्यात्व न होता तो क्रमविकास उन विद्यार्थियों की प्रगति के जैसा होता जो धीरे-धीरे अज्ञान से अधिक ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परंतु मिथ्यात्व ही है जो विकृति लाता है, जो असत्य को सत्य के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए यदि बालक गणित में कोई गलत हल करता है तो वह है अज्ञान, परंतु यदि वह गलती बताने पर भी अपने ही हल को सही सिद्ध करने पर अड़ा रहता है, तो यह है मिथ्यात्व। अतः पृथ्वी के विकास की किसी अवस्था विशेष पर इस मिथ्यात्व के तत्त्व को डाला गया था जो कि श्रीअरविन्द व श्रीमाताजी के अनुसार अतिमानसिक अवतरण के बाद समाप्त हो जाएगा। तब पृथ्वी पर विरोधी शक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ऐसा होने से क्रमविकास में हमें आज जो विषमताएँ दिखाई देती हैं, वे न रहेंगी और यह बड़े ही सुचारू रूप से गति कर सकेगा। और जब यह विकृत करने वाला तत्त्व न होगा तो सत्ता का प्रत्येक स्तर सहज रूप से अपने-आप को अभिव्यक्त करके अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच सकेगा, हालाँकि हमारे लिए इसकी परिकल्पना करना सहज ही संभव नहीं है कि प्राणिक और मानसिक जगत् किस प्रकार अपनी विराट् संभावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे जो कि वर्तमान में केवल अपनी क्षुद्र वृत्ति की पूर्ति के ही साधन बने हुए हैं।
इस सब में मुख्य बात यह है कि अधिकांश मनुष्यों की प्रकृति में दैवी और आसुरी प्रकृति के मिश्रण होते हैं। कुछ थोड़े मनुष्यों में दैवी गुण प्रबल होते हैं और कुछ में आसुरी। परंतु बहुत विरले ही हैं जिनमें कि इन वृत्तियों का पूर्ण अधिग्रहण हो जाता है। हमारे पुराणों आदि में हम इन्हीं दैवी और आसुरी वृत्तियों या प्रकृतियों द्वारा पूर्ण रूप से अधिग्रहीत लोगों के बीच के संघर्ष के विषय में उल्लेख पाते हैं। जब दैवी अधिग्रहण होता है तब व्यक्ति धीरे-धीरे आत्म-रूपांतर करके उत्तरोत्तर ऊर्ध्व गति करता है। परंतु आसुरी प्रभाव में व्यक्ति पहले धीरे-धीरे आसुरी वृत्तियों की ओर मुड़ने लगता है। ऐसे में वह धीरे-धीरे दूसरों के दुःख-दर्द के प्रति मुड़न्वेदनशील होने लगता है, किन्हीं भी सुंदर, शुभ चीजों के प्रति सचि खो बैठता है। उसमें गहरे भावों के प्रति कोई संवेदन नहीं रहता। और पूर्ण अधिग्रहण तब होता है जब वे आसुरी वृत्तियाँ व्यक्ति के चैत्य पुरुष को बिल्कुल दबा देने और, उससे भी अधिक, उसे निकाल बाहर कर देने में सफल हो जाती हैं। एक बार चैत्य के बाहर निकल जाने पर निष्कंटक रूप से आसुरी सत्ताओं का अधिग्रहण हो जाता है। श्रीमाताजी की पुस्तकों से हमें पता लगता है कि स्टालिन संभवतः जन्म से ही आसुरी था अर्थात् जन्म से ही उसमें चैत्य पुरुष नहीं था जबकि हिटलर का तब धीरे-धीरे पूर्ण अधिग्रहण हो गया जब उन सत्ताओं ने उसके चैत्य को दबाकर अपना अधिकार जमा लिया।
महाभारत के वन पर्व के एक प्रसंग में हम इस दैवी और राक्षसी प्रवृत्ति और उनके अधिग्रहण का एक बहुत ही सटीक उदाहरण पाते हैं। जब दुर्योधन को गंधर्व पकड़ कर ले गए और उसे बंदी बना लिया तब अर्जुन ने उसे उनसे मुक्त कराया। इससे दुर्योधन को बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अन्न-जल त्याग कर प्राण त्यागने का प्रण ले लिया। हालाँकि कर्ण ने अनेक प्रकार की नीतिपूर्ण बातों से उसे मनाने का प्रयास किया परंतु वह नहीं माना। तभी निम्नतर जगतों के दैत्यों और राक्षसों ने बुलाकर दुर्योधन को समझाया कि उसे आसुरी कायर्यों का निमित्त और यंत्र बनना है और दैवी प्रकृतिसंपन्न पांडवों से युद्ध कर उन्हें परास्त करना है इसलिए उसका जीवित रहना आवश्यक है। इस प्रकार उनकी बातों में आकर वह मान गया और अधिकाधिक आसुरी वृत्तियों का यंत्र बन गया।
इस वृत्तांत के माध्यम से हमें यह शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है कि ऐसी आसुरी सत्ताएँ हैं जो मनुष्य को अपना यंत्र बना लेती हैं, उन्हें अधिकृत कर लेती हैं और संसार में उनके द्वारा भगवद्विरोधी कार्यों को अंजाम देती हैं। परंतु ये सारे विषय बहुत ही जटिल हैं और इनके संबंध में कुछ मोटे संकेतों के अतिरिक्त अधिक कुछ सामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते। केवल इतना कह सकते हैं कि दो प्रकार को प्रकृतियाँ होती हैं - दैवी और आसुरी जिनमें से दैवी प्रकृति संपत्र लोग भगवान् के यंत्र होते हैं और दूसरे वाले उनकी क्रिया में बाधक होते हैं। परंतु एक अधिक गहरे दृष्टिकोण से देखने पर दोनों की ही क्रिया का कुल परिणाम भागवत् संकल्प की अभिव्यक्ति ही होता है। आसुरी प्रवृत्ति मैं भी अपने भीतर कहीं न कहीं यह बोध होता है कि उसका कल्याण भगवान् के विरोध के कारण ही हो सकता है। रावण आदि के संबंध में भी हमें पता लगता है कि भीतर से वे जानते थे कि भगवान् से द्वेष और विद्रोह करने से ही उनका कल्याण हो सकता है और वास्तव में ही उन्हें अंत में योगियों के लिए भी दुर्लभ सद्गति प्राप्त हुई।
श्रीभगवान् उवाच
अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।
दानं दमश्व यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १॥
१. श्रीभगवान् ने कहाः अभय, प्रकृति की शुद्धि, ज्ञानयोग में दृढ़ता, दान, आत्मसंयम और यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या, तथा स्पष्टवादिता।
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ।। २।।
२. दूसरों को पीड़ा न पहुँचाना, सच्चाई, क्रोध न करना, त्याग, शान्ति, दोष-दृष्टि से विरत, समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, लोभ न करना, मृदुता, विनम्रता, और दृढ़ता (चपलता से रहित)।
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ।। ३।।
३. तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह तथा अभिमान विहीनता – ये सब हे भारत! उनके गुण या संपदाएँ हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न हो जन्म ग्रहण करते हैं।
दम्भो दर्पो ऽभिमानश्व क्रोधः पारुष्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ।। ४।।
४. हे पार्थ। दम्म, दर्प और अभिमान, क्रोध और उसके साथ ही कटुता ता अज्ञान, हे पार्थ! उनके गुण या संपदाएँ हैं जो आसुरी प्रकृति से संपण तो जन्म ग्रहण करते हैं।
दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ।। ५।।
५. दैवी संपदाएँ मोक्ष की ओर ले जानेवाली कही गई हैं और आसुरी संपदाएँ बंधन की ओर। हे पाण्डव ! शोक मत कर, तेरा दैवी प्रकृति से संपन्न जन्म हुआ है।
-----------------------------
*...इसकी मृदुता, आत्म-त्याग और आत्म-संयम...समस्त दुर्बलता से मुक्त होते हैं: इसमें होता है तेज और आत्मबल, घृति या दृढ़ संकल्प, न्याय के अनुसार तथा सत्य और अहिंसा के अनुसार जीवन-यापन करने वाली आत्मा की निर्भयता, तेजः, अभयम्, धृतिः, अहिंसा, सत्यम्। दैवी संपदा से संपन्न मनुष्य की समस्त सत्ता एवं समस्त प्रकृति पूर्ण रूप से शुद्ध होती है; उसके अंदर ज्ञान-पिपासा और ज्ञानयोग में दृढ़ एवं स्थिर प्रतिष्ठा होती है।
श्रीगुरु कहते हैं कि अर्जुन देव-प्रकृति का है। उसे यह विचार करके शोक करने की आवश्यकता नहीं कि युद्ध और वध को अंगीकार करने से वह आसुरी आवेगों के अधीन हो जाएगा। जिस कार्य पर सब कुछ निर्भर करता है, जो युद्ध अर्जुन को करना है, जिसमें देहधारी ईश्वर उसके सारथि हैं और जगत् के प्रभु ने काल-पुरुष के रूप में प्रकट होकर जिसके लिए आदेश दिया है, वह धर्म के राज्य, सत्य, सदाचार और न्याय के साम्राज्य की स्थापना का संघर्ष है। वह स्वयं देवप्रकृति में उत्पन्न हुआ है; उसने अपने अन्दर सात्त्विक स्वभाव का विकास किया है, यहाँ तक कि अब वह उस अवस्था में पहुँच गया है जहाँ वह उच्च रूपांतर के योग्य है तथा त्रैगुण्य से और इसलिए सात्त्विक प्रकृति से भी मुक्ति लाभ करने में समर्थ है।
द्वौ भूतसर्गों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ।। ६।।
६. इस लोक में दो प्रकार के प्राणी सृष्ट होते हैं, दैवी और आसुरिक; दैवी स्वभाववालों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जा चुका है। हे पार्थ! अब आसुरिक स्वभाव वालों का वर्णन तू मुझसे सुन।
देव और असुर का भेद सारी-की-सारी मनुष्यजाति को समाविष्ट नहीं करता, यह इसके सभी व्यक्तियों पर कठोर रूप से प्रयोज्य नहीं है और न ही मनुष्यजाति के नैतिक या आध्यात्मिक इतिहास की सब अवस्थाओं में अथवा वैयक्तिक विकास के सभी चरणों में तीव्र और सुनिश्चित रूप से पाया जाता है। तामसिक मनुष्य, जो संपूर्ण जाति का इतना बड़ा भाग है, गीता में जिस प्रकार श्रेणियों का वर्णन है उस अनुसार किसी भी श्रेणी के अन्दर नहीं आता, हालाँकि उसके अंदर अल्प मात्रा में दोनों ही तत्त्व हो सकते हैं और यद्यपि अधिकांश में वह डरते-डरते निम्नतर गुणों की ही सेवा करता है। सामान्य मनुष्य साधारणतः एक मिश्रण होता है; परंतु कोई एक या दूसरी प्रवृत्ति अधिक सुनिश्चित होती है, वह उसे प्रधान रूप से राजस-तामसिक या सात्विक-राजसिक बनाती चली जाती है और ऐसा कहा जा सकता है कि वह उसे दैवी निर्मलता या दानवी विक्षुब्धता में से किसी एक परिणति के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि, यहाँ गुणात्मिका प्रकृति के विकास में एक प्रकार की विशेष परिणति ही गीता का लक्ष्य है, जैसा कि मूल में किये गये वर्णनों से स्पष्ट पता लग जाएगा। एक ओर तो सत्त्वगुण का उन्नयन, अजन्मे देवता का उत्कर्ष या प्राकट्य हो सकता है, दूसरी ओर प्रकृतिगत जीव के रजोगुण का उन्नयन एवं असुर का पूर्ण प्रादुर्भाव हो सकता है। इनमें से एक तो मोक्ष की उस गति की ओर ले जाता है जिस पर गीता अब बल देनेवाली है; इसके द्वारा सत्त्वगुण से बहुत ऊपर उठ जाना तथा भागवत् सत्ता के साधर्म्य में रूपांतरित होना संभव हो जाता है, विमोक्षाय। दूसरा हमें इस विश्वगत संभावना से दूर ले जाता है तथा हमारे अहं-बंधन को बड़ी तेजी से बढ़ाता है। इस समस्त भेद का मर्म यही है।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥
७. आसुरिक प्रकृति वाले मनुष्य कर्म करने की सच्ची विधि को और कर्म से निवृत्त होने की विधि को नहीं जानते; उनमें न शुचिता होती है, न सदाचार और न ही सत्य।
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ।। ८।।
८. वे कहते हैं कि "यह जगत् ईश्वर रहित है, असत्य है, निराधार है, केवल परस्पर संयोग के द्वारा उद्भुत है, इसका एकमात्र हेतु कामना है और कुछ नहीं।"
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।। ९।।
९. दृढ़तापूर्वक इस दृष्टि को बनाए रखते हुए, अल्पबुद्धि, उग्र और पाप कमों को करने वाली ये नष्ट अथवा भ्रष्ट आत्माएँ जगत् के नाश के लिए उसके शत्रुओं के रूप में उत्पन्न होती हैं।
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।
मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवर्तन्ते ऽशुचिव्रताः ।। १०।।
१०. अपूरणीय या अतृप्य कामना, दम्भ, दर्प और अतिशय अभिमान में लिए होकर, मूढ़तावश मिथ्या मतों को रखते हुए, अशुद्ध निश्चयों को धारण करके वे जगत् में कर्म करते हैं।
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्विताः ।। ११ ।।
११. ऐसी असंख्यों दुश्चिंताओं से ग्रस्त जो केवल उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होंगी, कामनाओं की तृति को ही परम लक्ष्य मानते हुए, और इस विषय में निश्चित रहते हुए कि बस ऐसा ही है।
आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ।। १२॥
१२. सैंकड़ों आशारूप पाशों से बंधे हुए, कामना और क्रोध के वशीभूत, कामना की तृप्ति के लिये अन्यायपूर्वक घन का संचय करने के लिये प्रयास करते रहते हैं।
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ।। १३।।
१३. "आज मैंने इस काम्य पदार्थ को प्राप्त कर लिया है, कल उस दूसरे पदार्थ को प्राप्त करूंगा; इतना धन मेरे पास आज है, कल मैं और अधिक प्राप्त कर लूंगा।
असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ।। १४ ।।
१४. "अपने इस शत्रु को मैंने मार डाला है और शेष दूसरों को भी मैं मार डालूंगा; मैं प्रभु हूँ, मैं उपभोग करने वाला हूँ, मैं सर्वसंपन्न या सिद्ध, बलवान् और सुखी (भाग्यशाली) हूँ;
आढधो ऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।। १५।।
१५. मैं धनवान् हूँ, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान करूंगा, मैं आमोद-प्रमोद करूँगा", इस प्रकार अज्ञान से विमूढ़ होकर;
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।। १६ ।।
१६. अनेक विचारों से विश्नांत होकर भटकते हुए, मोह जाल में फंसे हुए और अपनी कामनाओं की तृप्ति और भोगों में आसक्त वे मनुष्य एक अपवित्र नरक में गिरते हैं।
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ।। १७।।
१७. अपने-आपको बड़ा माननेवाले, ढीठ, धन और मान के नशे में चूर, वे दंभपूर्वक ऐसे यज्ञ करते हैं जो कि केवल नाम के ही यज्ञ होते हैं और विधिपूर्वक यज्ञ नहीं होते।
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः ।
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ।। १८।।
१८. अहंकार, बल, दर्प, कामना और क्रोध के वशीभूत ये विद्वेषपूर्ण लोग अपने स्वयं के शरीरों में और दूसरों के शरीरों में स्थित मुझ ईश्वर की निंदा (अवज्ञा) करते हैं।
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ।। १९।।
१९. इन पापी और क्रूर द्वेषियों को, इन (नीच-से-नीच) नराधमों को मैं निरंतर संसार में आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ।
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ।। २० ।।
२०. हे कौन्तेय! अनेक जन्मों तक आसुरी योनि को प्राप्त करते हुए वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं होते और आत्म-प्रकृति की निम्नतम अवस्था में गिरते जाते हैं।
यह जो जीवंत वर्णन है इसके द्वारा द्योतित भेद का पूरा महत्त्व स्वीकार करते हुए भी, इसका जितना अर्थ है उससे अधिक इसमें से बलपूर्वक निकालना उचित नहीं। जब यह कहा जाता है कि इस जड़ जगत् में, देव और असुर, दो प्रकार की जीव-सृष्टि पायी जाती है, तो इसका यह अर्थ नहीं होता असुर ने बर ने आरंभ से ही मानव-जीवों को इसी प्रकार का बनाया है और कित एव, प्रकृति के अंदर प्रत्येक की जीवनधारा अटल रूप से निश्चित है, ने ही इसका यह अर्थ होता है कि सबकी एक कठोर आध्यात्मिक पूर्वनिराले तय है और जिन लोगों को भगवान् ने आरंभ से ही त्याग रखा है वे उनके द्वारा अंधे बना दिये जाते हैं, ताकि उन्हें शाश्वत विनाश तथा नरक की अपवित्रता में धकेला जा सके। सभी जीव भगवान् के सनातन अंश हैं, जैसे देवता वैसे असुर भी; सभी मोक्ष लाभ कर सकते हैं: यहाँ तक कि घोर-से-घोर पापी भी भगवान् की ओर मुड़ सकता है। परंतु प्रकृति के अंदर जीव का विकास एक साहसपूर्ण कर्म, एक महाअभियान है जिसमें स्वभाव तथा स्वभावनियत कर्म सदा ही प्रधान शक्तियाँ होती हैं; और यदि जीव के स्वभाव की अभिव्यक्ति में कोई अति, उसकी क्रीड़ा में कोई अव्यवस्था सत्ता के धर्म को कुटिल पथ को ओर फेर दे, यदि राजसिक गुणों को प्रधानता दी जाए, सत्त्व का हास करके उनका विकास किया जाए, तो निश्चय ही, कर्म-प्रवृत्ति तथा उसके परिणाम उस सत्त्वगुण के उत्कर्ष में परिसमाप्त नहीं होते जो मोक्ष की गति में समर्थ है, अपितु वे निम्न प्रकृति के विकारों की पराकाष्ठा में ही परिसमाप्त होते हैं। यदि मनुष्य इस भ्रांत पथ पर चलना बंद नहीं करता तथा इसे त्याग नहीं देता तो अंततः उसके अंदर असुर पूर्णरूपेण जन्म ले लेता है, और जब एक बार वह ज्योति एवं सत्य से प्रबल रूप से पराङ्गमुख हो जाता है, तो अपने अंदर दिव्य शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग होने के कारण ही वह फिर अपने पतन की घातक गति को तब तक नहीं उलट सकता जब तक वह उन गहरे गतौँ की थाह नहीं ले लेता जिनमें कि वह पतित हुआ है, जब तक वह उनके तल तक नहीं पहुँच जाता और यह नहीं देख लेता कि यह मार्ग उसे कहाँ ले आया है, कैसे इसने उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया है तथा व्यर्थ में गँवा दिया है और कैसे वह स्वयं भी जीव-प्रकृति की निम्नतम अवस्था में गिर गया है, जो कि नरक है। जब वह यह सब समझकर ज्योति की ओर मुड़ जाता है केवल तभी गीता का यह दूसरा सत्य उसके सामने आता है कि अधम से अधम साथी भी, अत्यंत अपवित्र एवं घोर दुराचारी भी ज्यों ही अपने अंतःस्थ परमेश्वर का भजन और अनुसरण करने की ओर झुकता है त्यों ही उसका उद्धार हो जाता है। तब केवल उस झुकाव के द्वारा ही वह अत्यंत शीघ्र सात्त्विक मार्ग पर पहुँच जाता है जो पूर्णता और मुक्ति की ओर ले जाता है।
---------------------------------------
* इन दो प्रकार के सृष्ट जीवों के भेद का पूर्ण सत्य उन अतिभौतिक स्तरों में होता है जहाँ आध्यात्मिक क्रमविकास का नियम गति को नियंत्रित नहीं करता। जैसे देवताओं के लोक हैं, वैसे असुरों के भी लोक हैं, और हमारे पीछे अवस्थित इन लोकों में अपरिवर्तनीय प्रकार की सत्ताएँ होती हैं जो विश्व की प्रगति के लिए आवश्यक पूर्ण दिव्य सृष्टि-लीला को सहका देती हैं और सत्ता के इस भौतिक स्तर में भूतल पर तथा मनुष्य के जीवन और प्रकृति पर अपना प्रभाव भी डालती हैं।
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ।। २१ ।।
२१. काम, क्रोध और लोभ ये नरक के त्रिविध द्वार हैं जो जीव के नाश की ओर ले जाने वाले हैं: इसलिये मनुष्य इन तीनों का परित्याग करे।
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैत्रिभिर्नरः ।
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ।। २२।।
२२. हे कौन्तेय! अन्धकार के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ मनुष्य अपनी आत्मा के लिए जो कल्याणकारी है उसका साधन करता है और परम गति या पद को प्राप्त हो जाता है।
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ।। २३ ।।
२३. जो मनुष्य शास्त्र के नियम की अवहेलना करके अपनी कामनाओं के आवेगों के अनुसार आचरण करता है, वह मनुष्य न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और न परम गति या स्थिति को।
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।। २४।।
२४. इसलिये किस कर्म को करना चाहिये और किसे नहीं करना चाहिये इसका निर्णय करने के लिये तेरे लिये शाख ही प्रमाण होने चाहिए। अतः शाख ने क्या विधान बतलाया है उसे जानकर इस संसार में तुझे अपना कर्म करना चाहिये।
कामना के नियम का अनुसरण करना हमारी प्रकृति का सच्चा विधान नहीं है; इसके कर्मों का एक अधिक उच्च और न्यायसंगत आदर्श भी है। परंतु वह कहाँ निहित है अथवा उसे कैसे प्राप्त किया जाए? पहली बात यह है कि मनुष्यजाति इस न्यायोचित और उच्च विधान की खोज सदा ही करती रही है और जो कुछ उसने उपलब्ध किया है वह उसके शास्त्र में लिपिबद्ध है, वह शास्त्र है ज्ञान और विज्ञान का विधान, नैतिकता, धर्म तथा श्रेष्ठ सामाजिक जीवन का विधान, मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति के साथ हमारे यथार्थ संबंधों का रीति-रिवाजों का समूह नहीं है अच्छे होते हैं तो कुछ खराब, और जिनका अनुसरण तामसिक मनुष्य हा अच्छे होतरवश रूढ़िबद्ध मन बिना समझे-बूझे ही करता है। शाख वह ज्ञान और शिक्षा है जो अंतर्बोध, अनुभव और प्रज्ञा के द्वारा प्रतिष्ठित है, शाख है जीवन की विद्या, कला और आचारनीति, और साथ ही वे श्रेष्ठतम आदर्श जो मनुष्यजाति को उपलब्ध हैं। जो अर्द्ध-प्रबुद्ध मनुष्य शास्त्र के नियमों का पालन करना छोड़कर अपनी अंध-प्रेरणाओं एवं कामनाओं के मार्गनिर्देश का अनुसरण करता है वह इन्द्रिय-तृप्ति तो प्राप्त कर सकता है, पर सुख नहीं, क्योंकि आंतरिक सुख की प्राप्ति तो केवल समुचित प्रकार से जीवन यापन करने से ही हो सकती है। वह पूर्णता की ओर नहीं बढ़ सकता, सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता। पशु-जगत् में सहज-प्रवृत्ति और कामना का विधान प्रमुख नियम प्रतीत होता है, परंतु मनुष्य का मनुष्यत्व सत्य, धर्म, ज्ञान और यथोचित जीवनधारा का अनुसरण करने से ही विकसित होता है। इसलिए पहले उसे उस शास्त्र के अनुसार, लोकसम्मत सत्य-विधान के अनुसार आचरण करना होगा जिसे उसने अपने निम्नतर अंगों को अपनी बुद्धि तथा ज्ञानपूर्ण संकल्प के द्वारा नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया है, उसी को उसे अपने आचार-व्यवहार, कार्य-कलाप तथा कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का निर्णय करने के लिए प्रमाणरूप मानना होगा। और यह उसे तब तक करना होगा जब तक अंधप्रेरित कामनात्मक प्रकृति आत्म-संयम के अभ्यास के द्वारा शिक्षित नहीं हो जाती, क्षीण होकर दब नहीं जाती और जब तक मनुष्य पहले तो मुक्ततर ज्ञानपूर्ण मार्ग-दर्शन के लिए और फिर आध्यात्मिक प्रकृति के परमोच्च विधान एवं परम स्वातंत्र्य के लिए तैयार नहीं हो जाता।
क्योंकि, शास्त्र अपने साधारण रूप में ऐसा अध्यात्म-विधान नहीं है, यद्यपि अपने सर्वोच्च शिखर पर आध्यात्मिक जीवन का विज्ञान एवं शिल्प अर्थात् अध्यात्म-शास्त्र बन जाता है, - स्वयं गीता भी अपनी शिक्षा को एक उच्चतम और परम-गुह्य शास्त्र कहती है। अपने सर्वोच्च शिखर पर शाल सात्विक प्रकृति के अतिक्रमण की विध अपने सर्वोच्च कर देता है और आध्यात्मिक रूपांतर की साधना का विकास करता है। तो भी समस्त शाख नहीं। परम लक्ष्य तो है आत्मा का स्वातंत्र्य जिसमें जीव सब धर्मों का परित्याग कछ एक प्रारंभिक धर्मों के आधार पर निर्मित होते हैं: वे साधन होते हैं, लक्ष्य कर कर्म के अपने एकमात्र विधान के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ता है, सीधे कारवत् संकल्प के द्वारा कर्म करता है और दिव्य प्रकृति के स्वातंत्र्य में निवास करता है, धर्म में नहीं, अपितु आत्मा में निवास करता है। अर्जुन का अगला प्रश्न गीता की शिक्षा के इसी प्रकार के विकास का सूत्रपात करता है।
पशु-जगत् में भय और कामना के अतिरिक्त अन्य कोई चालक शक्ति नहीं होती। जिन मनुष्यों या समाजों में केवल कामना ही प्रमुख चालक शक्ति हो और कोई आत्म-अनुसंधान आदि का विधान न हो तो ऐसे मनुष्यों या समाजों को पशुतुल्य ही समझना चाहिये। मनुष्यत्व का अर्थ ही आत्म-अनुसंधान, आत्म-परिष्करण, संस्कारण आदि होता है। मानसिक या सात्त्विक विकास के साथ ही व्यक्ति जीवन के सच्चे विधान की खोज करता है। अपने आप को विकसित करने का, सुसंस्कृत बनाने का, उत्तरोत्तर विकास का, आंतरिक और बाह्य ज्ञान की खोज का प्रयास करता है। जब व्यक्ति शास्त्रों के वचनों के अनुसार, आत्मा के गहरे विधान के अनुसार जीवन को बदलने का प्रयास करता है तभी पशु से भिन्त्र होता है। जब व्यक्ति में कुछ-कुछ मानसिकता का विकास होता है और वह अपनी कामनाओं आदि के बारे में सचेतन होता है तब उन्हें शास्त्र के अनुसार संयत करने का प्रयास करता है। हालाँकि पाश्चात्य संस्कृति में सारा प्रयास अपनी कामनाओं की अधिकाधिक तृप्ति की ओर रहता है जिसमें सारे समाज की व्यवस्था इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर करने का प्रयास किया गया है कि वस्तुओं आदि का नियोजन इस प्रकार किया जाए कि किसी भी व्यक्ति की कामना की पूर्ति के अधिकारों का हनन हुए बिना सब अधिक से अधिक अपनी कामनाओं को तुष्ट कर सकें। परंतु भारतीय संस्कृति में सदा ही आत्मा का और उच्चतर विधान का बोध रहा है इसलिए भले ही यहाँ कामनाओं को अस्वीकार नहीं किया गया है परंतु उन्हें सदा ही शास्त्र के अंकुश में रखा गया है और मनुष्य को सदा ही उस उच्चतर उद्देश्य की ओर प्रेरित किया गया है। प्रत्येक मनुष्य के आंतरिक विकास को ध्यान में रखकर इस प्रकार एक अटूट स्तरानुगत विकास की व्यवस्था की गई जिसमें हर कोई अपनी वर्तमान स्थिति से अपने सच्चे लक्ष्य की ओर जा सके। सारे समाज को पग-पग पर ऐसे महत् विचारों, महान् आदशों, नीतियों, व्यवस्थाओं, विधि- विधानों, क्रिया-अनुष्ठानों, रूपकों आदि से परिवेष्टित कर दिया गया कि व्यक्ति को सदा ही हर क्षण अपने सच्चे लक्ष्य का न केवल स्मरण ही हो आता था अपितु उस ओर गति करने में भारी सहायता भी प्राप्त होती थी। साथ ही इस पूरी व्यवस्था में सदा ही यह नमनीयता रखी गई कि जो कोई इस सारे विधान को त्यागकर अपने आत्म-अनुसंधान में जाना चाहे वह इसके लिए स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रूप से अपने विकास के निजी मार्ग को खोज निकाले जिससे कि सारा ही समाज इससे लाभान्वित हो सके। इसी कारण हम महान् व्यक्तित्वों की एक अटूट परंपरा पाते हैं जिन्होंने सारे पूर्वनिर्मित विधानों को छोड़कर नवीन मार्गों का अनुसंधान और अन्वेषण किया।
इस प्रकार सोलहवाँ अध्याय 'दैवासुरसंपद्विभागयोग' समाप्त होता है।
सत्रहवाँ अध्याय
त्रिगुण, श्रद्धा, और कर्म
गीता व्यक्तिगत कामना की स्वच्छंदता के अनुसार किये जाने वाले कर्म में और शास्त्र के अनुसार किये जानेवाले कर्म में भेद कर चुकी है। शास्त्र शब्द से हमें जीवनसंबंधी उस सर्वसम्मत विद्या एवं कला को समझना होगा जो मनुष्यजाति के सामूहिक जीवन का, उसकी संस्कृति, धर्म एवं विज्ञान का, जीवन के सर्वश्रेष्ठ विधान की उसकी उत्तरोत्तर खोज का परिणाम है, – परंतु उस मनुष्यजाति के जीवन का परिणाम है जो अभी भी अज्ञान में गति कर रही है और एक अधूरे प्रकाश में ही ज्ञान की ओर अग्रसर हो रही है। व्यक्तिगत कामना का कर्म हमारी प्रकृति की असंस्कृत अवस्था से संबंध रखता है और वह अज्ञान या मिथ्या ज्ञान और एक अनियंत्रित या कुनियंत्रित राजसिक अहंकार से प्रेरित होता है। शास्त्र के द्वारा नियंत्रित कर्म बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक और धार्मिक संस्कृति का एक परिणाम होता है; वह एक प्रकार के यथोचित जीवन-यापन, सामंजस्य एवं समुचित व्यवस्था के लिए किये गये प्रयत्न का मूर्त रूप होता है, और स्पष्ट ही वह मनुष्य के सात्त्विक अंश का एक प्रयास होता है जो राजसिक तथा तामसिक अहंकार पर प्रभुत्व करने, उसे संयत और नियंत्रित करने के लिए अथवा, जहाँ इसे स्वीकार करना आवश्यक होता है वहाँ, इसका परिचालन करने के लिए किया जाता है; वह प्रयास परिस्थितियों के अनुसार कम या अधिक उन्नत या विकसित होता है। वह आगे की ओर एक कदम बढ़ाने का एक साधन होता है, अतएव मनुष्यजाति को पहले इसमें से गुजरना होगा और इस शास्त्र को अपने कर्म का विधान बनाना होगा बजाय अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की प्रेरणा का अनुसरण करने के..
मनुष्य की असंस्कृत प्रकृति निरंकुश प्रकार की होती है जिसमें वह पशु की भाँति अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, आवेगों आदि को अनियंत्रित रूप से पूरी करने की चेष्टा करता रहता है। जब मनुष्य समूहगत जीवन जीना आरंभ करता है तब उसे केवल निजी तुष्टियों को ही नहीं अपितु सामूहिक तुष्टियों को भी ध्यान में रखना होता है। तब किसी प्रकार के निरंकुश व्यवहार की बजाय उसे सामूहिक विधान के अनुसार आचरण करना होता है क्योंकि अहं की तुष्टि के बोध के साथ ही साथ उसमें यह बोध भी आ जाता है कि अपनी कामनाओं की पूर्ति का जितना अधिकार स्वयं उसे है उतना ही अधिकार अन्य दूसरों को भी का साथ ही सामूहिक जीवन में वह समूह से कुछ प्राप्त करता है और बदले में उसे अपना योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार घोर स्वार्थ और पाशविकता के जीवन की बजाय वह एक सामूहिक विधान के अनुसार जीवन यापन करने लगता है। जब धीरे-धीरे उसके मन का विकास होता है, उसकी सौंदर्यपरक आदि क्षमताओं का विकास होता है तब वह चीजों को करने के सही विधान को, उनके बीच के सामंजस्य को खोजने लगता है। चीजों को करने के उचित विधान को ही शास्त्र कहते हैं। धीरे-धीरे भौतिक, प्राणिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रकृतियों का अवलोकन कर वह उन सभी के सही विधानों को खोजने और उन्हें शास्त्र के रूप में जीवन में प्रयुक्त करने का प्रयास करता है। भौतिक प्रकृति के अवलोकन से उसे कृषि आदि का, वस्तुओं के साथ उचित व्यवहार का, भौतिक ऊर्जा के समुचित नियोजन आदि के विधान या शास्त्र का पता लगता है। प्राणिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रकृतियों के अवलोकन से उसे परस्पर संबंधों के सही विधान का, भावनाओं आदि के नियमन का, आचार-व्यवहार के विधान का, विचारों के सौंदर्य का, चीजों के बीच के सामंजस्य का बोध होता है। इस प्रकार केवल निरंकुश स्वार्थपूर्ति की बजाय व्यक्ति उचित विधान या शास्त्रों के अनुसार जीवन-यापन करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह सात्त्विक प्रकृति द्वारा निरंकुश राजसिक और तामसिक प्रकृति को संयमित करने का उपाय है। शास्त्र की सहायता से व्यक्ति जब अपनी स्वेच्छाचारी वृत्तियों पर लगाम लगाने में कुछ-कुछ सफल होता है तब संभव है कि उसकी सहायता से वह कुछ-कुछ धर्म और अध्यात्म की दिशा में भी गति करे। परंतु मनुष्यजाति को अपने विकासक्रम में इस अवस्था से गुजरना ही होता है। इससे गुजर कर ही वह किसी अधिक सुसंस्कृत अवस्था तक पहुँच सकती है।
परंतु हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य के अंदर एक अधिक स्वच्छंद प्रवृत्ति भी है जो उसकी कामनाओं के अनुसरण करने से तथा विधान को, निर्धारित विचार को, शास्त्र के सुरक्षित नियामक विधि-विधान को स्वीकार करने के संकल्प से भिन्न है। जहाँ व्यक्ति को प्रायः ही, वहीं समाज को अपने जीवन के किसी भी क्षण में शास्त्र से मुँह मोड़ते, उससे ऊबते देखा जाता है, वह अपने संकल्प और श्रद्धा-विश्वास के उस रूप को छोड़ देता है और किसी अन्य विधान की खोज में निकल पड़ता है जिसे वह अब जीवन-यापन के यथार्थ विधान के रूप में स्वीकार करने तथा अस्तित्व के एक अधिक महत्त्वपूर्ण या उच्चतर सत्य के रूप में मानने की ओर अधिक झुका हुआ होता है। यह उस समय हो सकता है जब प्रचलित-प्रतिष्ठित शास्त्र कोई जीवंत वस्तु नहीं रहता और रीति-रिवाजों और लोकाचारों के समूह में अपभ्रष्ट या रूढ़ हो जाता है। अथवा यह इसलिए हो सकता है कि शास्त्र अपूर्ण पाया जाता है या अपेक्षित प्रगति के लिए और अधिक उपयोगी नहीं पाया जाता; एक नया सत्य, जीवन-यापन का एक अधिक पूर्ण विधान अनिवार्य हो जाता है... यह आंदोलन व्यक्ति से प्रारंभ होता है जो कि वर्तमान विधान से अब और अधिक संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह देखता है कि वह विधान उसके अपने-आप के और जगत्-अस्तित्व के संबंध में उसकी धारणा एवं विशालतम या तीव्रतम अनुभूति से अब और मेल नहीं खाता और इसलिए वह उस पर विश्वास तथा आचरण करने के लिए उसमें अपने संकल्प को पहले की तरह नियोजित नहीं कर सकता। वह उसके आंतरिक भाव या स्थिति से मेल नहीं खाता, उसके लिए अब वह 'सत्' अर्थात् कोई ऐसी वस्तु नहीं रहता जिसका वस्तुतः अस्तित्व हो, न ही वह उसके लिए यथार्थ विधान, उच्चतम या सर्वश्रेष्ठ या यथार्थ रूप में कल्याणकर रहता है; वह उसकी सत्ता या सर्व सत्ता का सत्य एवं विधान नहीं रहता। शास्त्र व्यक्ति के लिए एक निर्वैयक्तिक वस्तु होता है, और वह निर्वैयक्तिकता ही उसे व्यक्ति के अंगों के संकीर्ण वैयक्तिक विधान के ऊपर उसकी प्रामाणिकता प्रदान करती है; पर इसके साथ ही वह शास्त्र समष्टि के लिए निजी होता है और उसकी अनुभूति, उसकी संस्कृति या उसकी प्रकृति की उपज होता है। वह अपने समस्त रूप और भाव में आत्मा की परिपूर्णता का आदर्श विधान या हमारी प्रकृति के स्वामी का सनातन विधान नहीं होता, भले ही उसके अंदर उस अति महत्तर वस्तु के संकेत, तैयारी, प्रकाशप्रद आभास कम या अधिक मात्रा में क्यों न विद्यमान हों। और व्यक्ति समष्टि को अतिक्रम कर उससे आगे बढ़ा हुआ हो सकता है और एक महत्तर सत्य, एक प्रशस्ततर मार्ग, प्राण-पुरुष के एक गंभीरतर प्रयोजन के लिए तैयार हो सकता है।
अतः व्यक्ति की इच्छाओं, कामनाओं, अंध प्रवृत्तियों आदि को नियंत्रित करने में शास्त्र की अत्यधिक उपयोगिता है। परन्तु मनुष्य के अन्दर इन वृत्तियों के अतिरिक्त ऐसे भी भाग हैं जो बहुत गहराइयों में निवास करते हैं। अतः जिनमें ये भाग सक्रिय होते हैं और बाहरी प्रकृति निरव अपना प्रभाव और प्रकाश डालते हैं उन्हें समाज के निर्धारित विधान पर अपना प्रभाव अत्यंत संकीर्ण या अनुपयोगी लगने लगते हैं या फिर या शाख भारिक पुकार से विसंगत लगने लगते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी विधान हमारे गहरे भागों पर बाध्यकारी नहीं हो सकते। वे तो तभी तक उपयोगी होते हैं जब तक कि व्यक्ति इतना अपरिपक्व होता है कि तुझे इन बाहरी सहारों की आवश्यकता होती है। परंतु जब एक बार कुछ गहरे भाग सक्रिय हो जाते हैं तब उनके प्रभाव से व्यक्ति गोचर प्रतीतियों के भीतर के सत्य का अन्वेषण करने लगता है। और यदि व्यक्ति में यह अन्वेषण गहन हो और साथ ही उसमें पर्याप्त सामर्थ्य हो तो वह प्रतिष्ठित शास्त्रों का विरोध कर अपने ही नये मार्ग की खोज और निर्माण कर सकता है। सामान्यतः ऐसे ही लोग समाज में किन्हीं भी महान् परिवर्तनों के सूत्रधार होते हैं। जितने भी महान् व्यक्तित्व हुए हैं उन सब के विषय में यही एक बात सर्वसामान्य रहती है कि या तो उनकी आत्मा प्रतिष्ठित शास्त्रों से बँधना स्वीकार नहीं करती और उनका विरोध करती है या फिर यदि वे उन्हें स्वीकार करते भी हैं तो अपने ही विशिष्ट तरीके से उन्हें सर्वथा अतिक्रम कर जाते हैं और अपने ही नए पथ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार समय-समय पर समाज को एक नई दिशा मिलती है तथा जीवन जीने के तरीकों में अधिक समृद्धता आती है। परंतु शास्त्र के प्रति यह ऊब किसी व्यक्ति में ही नहीं अपितु समष्टिगत रूप से पूरी जाति में भी आ सकती है। कितनी ही बार हम किसी राष्ट्र में पूरी की पूरी शासन प्रणाली के विरुद्ध आम विरोध देखते हैं जिसमें केवल कोई व्यक्ति ही नहीं अपितु पूरा समाज ही तय विधानों के विरोध में उतर आता है और उसे त्याग कर किसी नए विधान की खोज और स्थापना करता है और जब उस विधान की भी समय सीमा और उपयोगिता समाप्त हो जाती है तब वह भी किसी न किसी तरह त्याग दिया जाता है। विश्व का सारा इतिहास हमें इस प्रवृत्ति का पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करता है। अतः हमारे ऊँचे से ऊँचे विधान भी अपने समय पर तो प्रचलन में रहते हैं परंतु जब उनका समय समाप्त हो जाता है और वे रूढ़ बन जाते हैं तो किसी नए विधान के द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। चूंकि पार्थिव अभिव्यक्ति क्रमविकासमय है इसलिए यह सभी चीजें बदलती रहती हैं जिसके कारण जो चीज किसी समय विशेष पर व्यष्टि या समष्टि के लिए सहायक होती है वही कालांतर में आवश्यक नहीं कि सहायक बनी रहे अपितु एक समय के बाद वह आगे की प्रगति में बाधक सिद्ध होती है।
इसलिए हम यह आशा नहीं कर सकते कि एक गौतम बुद्ध शास्त्रों के अनुसार ही गति करें। या फिर समष्टिगत रूप से ऐसा संभव नहीं है कि अतीत में हुई फ्रांसीसी क्रांति को तथा पुनर्जागरण को रोका जा सके। इन सभी व्यष्टिगत और समष्टिगत उदाहरणों में हम देखते हैं कि एकाएक ही सारे समाज के मूल्यों का पुनर्गठन और नवनिर्माण हो जाता है। पुराने मूल्यों को नए मूल्यों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार हम सदा ही दो वृत्तियों को क्रियारत देखते हैं। एक वृत्ति है उचित विधान या शास्त्र के निर्माण की वृत्ति जो व्यक्ति और समाज को निरंकुश आचरण से रोकती है और उसे संस्कारित करती है और इसके साथ ही दूसरी वृत्ति है इन शास्त्रों में अधिक नमनीयता लाने की तथा इनका अतिक्रम करने की।
किंतु तब फिर एक ऐसे कर्म का सुनिश्चित आधार क्या होना चाहिए जो कामना के निर्देश तथा प्रचलित विधान दोनों से हटकर चलता है? क्योंकि, कामना के नियम का अपना एक प्रभुत्व होता है जो हमारे लिए अब और वैसे ही सुरक्षित या संतोषजनक नहीं रहता जैसा वह पशु के लिए होता है या फिर जैसा वह आदिम मानवता के लिए रहा होगा, परंतु फिर भी अपनी सीमा के भीतर यह हमारी प्रकृति के एक अति जीवंत भाग पर आधारित और उसके प्रबल संकेतों के द्वारा संपुष्ट होता है; इस धर्म अथवा शास्त्र के पीछे होते हैं चिर-प्रचलित विधान की समस्त प्रामाणिकता, पुराने समय में उसे मिली सफल अनुमोदन या स्वीकृति और एक सुनिश्चित अतीत-अनुभूति। किंतु यह नया प्रयास अज्ञात या अंशतः-ज्ञात की ओर एक शक्तिशाली अभियान, एक साहसिक विकास और एक नूतन विजय का स्वरूप रखता है, तो फिर वह कौन-से सूत्र का अनुसरण करे, वह कौन-सा मार्गदर्शक प्रकाश है जिस पर यह प्रयास निर्भर करे या भरोसा रखे या हमारी सत्ता के अंदर इसका दृढ़ आधार क्या हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि वह सूत्र और आधार हमें मनुष्य की श्रद्धा में मिलेगा; श्रद्धा अर्थात् जिसे वह अपने-आप के तथा सत्ता के सत्य के रूप में देखता या समझता है उस पर विश्वास करने तथा उसे जीने का संकल्प। दूसरे शब्दों में इस प्रयास का अर्थ है मनुष्य का अपने सत्य, अपने जीवन-विधान, अपनी पूर्णता और सिद्धि के पथ की उपलब्धि के लिए अपनी निज सत्ता के प्रति या फिर अपनी सत्ता या विश्व-सत्ता के अंदर विद्यमान किसी शक्तिशाली एवं बाध्यकारी वस्तु के प्रति पुकार करना। और सब कुछ निर्भर करता है उसकी श्रद्धा के स्वरूप के ऊपर, अपने अंदर या जिस विश्वात्मा का वह एक अंश या प्राकट्य है, उसके अन्दर विद्यमान जिस वस्तु के प्रति वह अपनी श्रद्धा अर्पित करता है उसके ऊपर और इसके द्वारा वह अपनी वास्तविक आत्मा तथा विश्व की आत्मा या उसकी वास्तविक सत्ता के कितना निकट पहुँचता है इस बात के ऊपर। यदि वह तामसिक, मूढ़ एवं तमसाच्छन्न है, यदि उसकी श्रद्धा अज्ञानयुक्त तथा संकल्प अक्षम है तो वह किसी भी यथार्थ वस्तु तक नहीं पहुँच पाएगा तथा अपनी निम्न प्रकृति में जा गिरेगा। यदि वह मिथ्या राजसिक प्रकाशों के प्रलोभन में पड़ गया तो वह अपने स्वेच्छाचारी संकल्प के द्वारा ऐसे उपमार्गों में भटक सकता है जो उसे दलदल या गह्वर की ओर ले जा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में उसके उद्धार का एकमात्र अवसर इस बात में है कि उसके अंदर सत्त्वगुण फिर से प्रबलता प्राप्त कर ले और वह उसके अंगों पर एक नयी ज्ञानदीप्त नियम-व्यवस्था लागू करे जो उसे उसके स्वच्छंद संकल्प की प्रचंड भ्रांति या उसके तमसाच्छन्न अज्ञान की जड़ भ्रांति से मुक्त कर देगी। इसके विपरीत, यदि उसकी प्रकृति सात्त्विक है और यदि उसे आगे बढ़ने के लिए सात्त्विक श्रद्धा एवं निर्देश प्राप्त है तो एक अब तक अनुपलब्ध उच्चतर आदर्शविधान उसे दृष्टिगोचर हो जाएगा जो उसे किन्हीं विरले प्रसंगों में सात्त्विक प्रकाश से भी ऊपर सत्ता और जीवन की उच्चतम दिव्य ज्योति एवं दिव्य प्रणाली की ओर कुछ दूर तो ले ही जा सकता है। क्योंकि यदि उसके अंदर सात्त्विक प्रकाश इतना प्रबल हो कि वह उसे अपनी चरम सीमा तक ले जाए तो वह उस सीमा से आगे बढ़कर भागवत्, विश्वातीत एवं निरपेक्ष सत्ता की किसी प्रथम रश्मि में प्रवेश के लिए मार्ग बनाने में समर्थ होगा। आत्म-अनुसंधान के सभी प्रयत्नों में ये संभावनाएँ विद्यमान हैं; ये इस आध्यात्मिक अभियान की शर्तें हैं।
अब हमें यह देखना है कि गीता अध्यात्म-शिक्षा और आत्म-साधना की अपनी पद्धति के अनुसार इस प्रश्न का कैसा समाधान करती है। क्योंकि अर्जुन तुरंत ही एक ऐसा संकेतात्मक प्रश्न करता है जिससे यह समस्या या इसका एक पक्ष उपस्थित होता है।
यह एक बड़ा ही मूलभूत प्रश्न है। कर्म का एक विधान तो कामना हो सकती है जिसका कि नियंत्रण शास्त्र के द्वारा और शास्त्र के आधार पर किया जाता है। परंतु जब शास्त्र का आधार छोड़ दिया जाए तब फिर वह कौनसा आधार हो जिस पर कि कर्म को प्रतिष्ठित किया जाए? और फिर उस कर्म के सही या गलत होने की कसौटी या मापदंड क्या हो? यह कसौटी है व्यक्ति की श्रद्धा जो निर्धारित करती है कि वह कर्म सही है या नहीं। इसी को गीता तीन भागों में विभाजित करके 'श्रद्धात्रयविभागयोगः का निरूपण करती है। इसी संदर्भ में वह कहती है कि वास्तव में जिसकी जो श्रद्धा होती है व्यक्ति उसी के अनुसार होता है और भविष्य में भी व्यक्ति वही होगा जो उसकी श्रद्धा होगी।
मनुष्य को जो श्रद्धा होती है अर्थात् अपनी सत्ता का जो सत्य महसूस होता है उसी के अनुसार वह अपने जीवन को ढालने का प्रयास करता है। इसी कारण समान ही परिवेश में पले-बढ़े होने पर भी भिन्न श्रद्धा होने पर व्यक्ति भिन्न-भिन्न जीवन व्यतीत करते हैं। उदाहरण के लिए किसी को अपने इष्ट में अपनी सत्ता का सत्य नजर आता है, किसी को अपने गुरु के अंदर वह सत्य दिखाई देता है, किसी अन्य को श्रद्धा के किसी अन्य पात्र में यह सत्य दिखाई देता है तो वह अपने जीवन को उस अनुसार दिशा प्रदान करने का प्रयास करता है और तब वही उसके कर्म का आधार बन जाता है। यदि यह श्रद्धा तामसिक या राजसिक प्रकार की हो तो दोनों ही उसे गर्त में ले जाती हैं। इनसे निकलने का उपाय है कि सात्त्विक श्रद्धा का विकास किया जाए। यदि किसी की प्रकृति सात्त्विक प्रकार की हो और उसमें सात्त्विक श्रद्धा हो तो यह संभावना है कि उसे एक ऐसे आदर्श के दर्शन हों जो उसे अब तक गोचर नहीं हुआ था और यह भी संभव है कि उस सात्त्विक श्रद्धा के प्रभाव से उसे किन्हीं विरले क्षणों में सात्त्विकता से भी ऊपर की ज्योति के दर्शन हों। इस प्रकार श्रीअरविन्द अपनी टिप्पणी में ये सारी संभावनाएँ प्रकट करते हैं जो उस व्यक्ति के साथ हो सकती हैं जो शास्त्र को छोड़कर किसी नए मार्ग के अनुसार चलने का प्रयास करता है।
प्रश्न : यहाँ श्रद्धा की जो बात कर रहे हैं उसमें समस्या क्या श्रद्धा में है या जिस चीज के ऊपर श्रद्धा रखी गई है, उसमें है?
उत्तर : समस्या श्रद्धा में नहीं अपितु उस माध्यम में है जिसके द्वारा वह अभिव्यक्त होती है। श्रद्धा तो अपने आप में सदा ही सही होती है परन्तु उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम पर निर्भर करता है कि वह कितने शुद्ध रूप में अभिव्यक्त हो पाती है।
प्रश्न : तो क्या इसका यह अर्थ है कि हमारी सत्ता के कुछ भाग उस श्रद्धा को स्वीकार नहीं करते?
उत्तर : इसमें स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है। उन भागों में अपने को उत्तर: के प्रति अतिशय आग्रह रहता है जिन्हें छोड़ने के लिए ने तौर से नहीं होते इसलिए श्रद्धा उसी के अनुरूप अभिव्यक्त होती है। तैयार में के लिए किसी धार्मिक व्यक्ति के अन्दर श्रद्धा उस धर्म की उदारखा के अन्दर ही अभिव्यक्त होती है क्योंकि उस व्यक्ति के लिए उस धर्म की सीमाओं को अतिक्रम कर जाना सहज नहीं होता। इसी कारण श्रद्धा की क्रिया प्रायः एक सीमा तक ही संपन्न हो पाती है और उसको स्वतंत्र क्रिया बहुत ही कम देखने को मिलती है। साथ ही, जिसे हम सामान्यतः श्रद्धा कहते हैं उसकी क्रिया भी तभी तक होती है जब तक कि व्यक्ति को उस सत्य के साक्षात् दर्शन न हुए हों। क्योंकि एक बार वह प्रत्यक्ष दर्शन होने के पश्चात् फिर श्रद्धा का स्वरूप वैसा नहीं रहता। तब वह व्यक्ति के लिए एक बिल्कुल सहज और निश्चित तथ्य बन जाती है। जिसे हम प्रायः श्रद्धा कहते हैं वह तो तभी तक रहती है जब तक कि व्यक्ति को वह सत्य केवल भीतर ही गोचर हुआ है परंतु बाहरी भागों को अभी भी श्रद्धा के रूप में ही उसे स्वीकार करना पड़ता है। परंतु जब एक बार वह सत्य गोचर हो जाता है तब फिर इसमें श्रद्धा की इस तरह की भूमिका नहीं रह जाती क्योंकि तब वह हमारी सत्ता का एक सहज तथ्य या वास्तविकता बन जाती है जिसे व्यक्ति बिना किसी संदेह की छाया के जीवन में अभिव्यक्त करता है।
अर्जुन उवाच
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ।। १॥
१. अर्जुन ने कहाः हे कृष्ण! जो मनुष्य शास्त्र के विधान का परित्याग कर के परन्तु श्रद्धा से परिपूर्ण होकर यज्ञ करते हैं, उनके अंदर भक्ति का वह एकनिष्ठ संकल्प (निष्ठा) किस प्रकार का है? वह सत्त्व है, रजस् है अथवा तमस् है?
श्रीभगवान् उवाच
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २॥
२. श्रीभगवान् ने कहाः देहधारियों की उनके स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा तीन प्रकार की होती है देह सारों को नजसिक और तामसिक। इनके बारे में तू सुन।
जब हम अपनी कामनाओं के अनुसार जीते हैं, उन्हीं के अनुसार होते और कर्म करते हैं तो वह हमारी उस श्रद्धा की ही एक अनवरत क्रिया होती है जो अधिकांशतः हमारी प्राणिक और भौतिक, तामसिक और राजसिक प्रकृति से संबद्ध होती है। और जब हम शास्त्र के अनुसार बनने, जीवन यापन करने और कर्म करने की चेष्टा करते हैं तो हम जिस श्रद्धा की निरंतर क्रिया के द्वारा अग्रसर होते हैं वह – यदि यह मान कर चलें कि वह कोई सामान्य श्रद्धा-विश्वास मात्र न हो तो - एक सात्त्विक प्रवृत्ति की होती है जो हमारे राजसिक और तामसिक भागों पर अपने को लादने के लिए सतत् रूप से प्रयास कर रही होती है। जब हम इन दोनों चीजों को छोड़ देते हैं और हमारे अपने खोजे हुए या हमारे निजी रूप से स्वीकार किये गए किसी आदर्श के अनुसार या सत्य की किसी अनूठी परिकल्पना के अनुसार बनने, जीवन यापन करने और कर्म करने का यत्न करते हैं तो वह भी उस श्रद्धा की एक निरंतर क्रिया होती है जो हमारे प्रत्येक विचार, संकल्प, भाव और कर्म पर निरंतर नियंत्रण रखनेवाले इन तीन गुणों में से किसी एक के अंतर्गत हो सकती है। और फिर, जब हम दिव्य प्रकृति के अनुसार बनने, जीने और कर्म करने का यत्न करते हैं, तब भी हमें श्रद्धा की सतत् क्रिया के द्वारा ही बढ़ना होता है; और यह श्रद्धा गीता के अनुसार उस सात्त्विक प्रकृति की श्रद्धा होनी चाहिये जो अपने आप की सुस्पष्ट सीमाओं की पराकाष्ठा तक पहुँच कर उन्हें अतिक्रम करने की तैयारी कर रही हो। परंतु इनमें से सभी चीजों में तथा इनमें से प्रत्येक में प्रकृति की कोई गतिशीलता या अवस्थान्तर अंतर्निहित है, ये सभी किसी आंतरिक या किसी बाह्य क्रिया को या फिर आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही क्रियाओं को मानकर चलती हैं। तो फिर इस क्रिया का स्वरूप क्या होगा? गीता हमारे 'कर्तव्यं कर्म' अर्थात् करने योग्य कर्म के तीन मुख्य तत्त्व बताती है, और ये हैं यज्ञ, दान और तप। क्योंकि जब अर्जुन द्वारा बाह्य और आंतरिक त्याग, 'संन्यास' और 'त्याग' में भेद के विषय में प्रश्न किया जाता है तब श्रीकृष्ण द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि इन तीन चीजों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, अपितु इन सभी को तो बराबर करते hat 5T रहना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे लिए 'कर्त्तव्यं कर्म' है और ये ज्ञानी मनुष्य को पवित्र करते हैं। दूसरे शब्दों में ये कर्म ही हमारी पूर्णता के साधन हैं। परंतु साथ ही ये अज्ञानी द्वारा अज्ञानपूर्वक या अपूर्ण ज्ञान के साथ किये जा सकते हैं।
वास्तव में, आरंभ में जब हमारी बाह्य सत्ता अपरिपक्व होती है, तथा विकसित या सुसंस्कृत नहीं होती, तब श्रद्धा को अपनी अभिव्यक्ति प्राणिक और भौतिक, तामसिक और राजसिक प्रकृति के अनुसार ही करनी होती है। इसमें व्यक्ति कामनाओं के आधार पर ही कर्म करता है। परंतु जब कुछ विकास होने पर वह निजी कामनाओं की तुष्टि हेतु कर्म करने की बजाय किसी श्रेष्ठ आदर्श के आधार पर कर्म करना चाहता है, उचित कर्म करना चाहता है तब यह सात्त्विक प्रकृति की क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को शास्त्रसम्मत आधार पर नियोजित करना चाहता है और उसके अनुसार अपनी निरंकुश भौतिक और प्राणिक प्रकृति पर कुछ-कुछ अंकुश लगाने का प्रयास करता है। हमारे तामसिक भाग सदा ही अपने क्षुद्र सुख-दुःख के अनुसार क्रिया करते हैं, राजसिक भाग अपनी प्राणिक वृत्तियों की, कामनाओं, लालसाओं, अपने अहं की तुष्टियों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। परंतु मनुष्य की सात्त्विक प्रकृति का प्रयास जीवन को किसी उचित विधान के अनुसार नियोजित करने का होता है और जब व्यक्ति सच्चाई के साथ इस ओर चलने का प्रयास करता है तब इससे उद्दण्ड निम्न प्रकृति की निरंकुश क्रिया पर बहुत कुछ लगाम लग जाती है।
परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शास्त्रसम्मत जीवन यापन न कर के अपने ही किसी अन्य विधान के अनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं। और शास्त्र विरोधी यह भाव किसी तामसिक प्रेरणा से प्रेरित हो सकता है, राजसिक प्रेरणा से प्रेरित हो सकता है या फिर सात्त्विक प्रेरणा से प्रेरित हो सकता है या फिर किन्हीं दो प्रेरणाओं के मिश्रण से हो सकता है। यही अर्जुन का प्रश्न था कि वह श्रद्धा तामसिक होती है या फिर राजसिक या सात्त्विक। इस विषय में श्रीअरविन्द कहते हैं कि यह श्रद्धा तीनों गुणों में से किसी एक या अधिक के अनुसार हो सकती है, यहाँ तक कि यह इन तीनों गुणों से परे की भी हो सकती है। और उस श्रद्धा के आधार पर ही व्यक्ति को अपने नवीन पथ पर अग्रसर होना होता है।
जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार गीता के विषयों को प्रायः उनके मूल व्यापक स्वरूप में न समझकर किसी सतही संकीर्ण तथा स्थूल अर्थ में लेने की भूल की जाती है उसी प्रकार यज्ञ, तप व दान को भी उनके मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ में न लेकर केवल एक बाहरी क्रिया के रूप में ही समझ लिया जाता है। यज्ञ, जो कि इस सृष्टि का एक मूलभूत विधान है जिसे किये बिना कोई रह ही नहीं सकता, उसे केवल कोई बाह्य आनुष्ठानिक यज्ञ ही मान लिया जाता है जबकि यज्ञ, तप और दान ऐसी मूलभूत चीजें हैं जिन्हें इस सृष्ट जगत् में कोई भी किये बिना रह ही नहीं सकता। यज्ञ, तप और दान का विधान तो इस जगत् के निर्माण में निहित है अतः भले व्यक्ति इन्हें सहर्ष करे या फिर इन्हें प्रकृति की बाध्यकारी शक्ति के द्वारा उस पर लादा जाए, परंतु किसी भी दशा में कोई भी इनसे बच नहीं सकता। इतना अवश्य है कि यदि व्यक्ति सहर्ष यह क्रिया करता है तो उसे इनका आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त होता है, जबकि यदि अवश रूप से प्रकृति द्वारा उससे वे कराए जाते हैं तो उसे उनका वह लाभ प्राप्त नहीं होता।
यज्ञ का अर्थ है परस्पर आदान-प्रदान के द्वारा पवित्र बनाना। जब व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं, कामनाओं को पूरा करना चाहता है तथा अन्य किसी से कोई सरोकार नहीं रखता तब वह तामसिक यज्ञ होता है। जब व्यक्ति केवल अपनी ही इच्छाओं आदि की पूर्ति पर केंद्रित रहने की बजाय दूसरों की सत्ता को भी स्वीकार करता है और उनके सुख-आराम के विषय में भी सोचता है और उसे यह भान होता है कि सामूहिक जीवन में यदि वह दूसरों से कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वयं भी कुछ योगदान करना होगा, जब इस भाव से व्यक्ति कर्म करता है तब यह राजसिक यज्ञ होता है। परंतु इन किन्हीं भी कारणों को छोड़कर जब व्यक्ति जो उचित है, श्रेष्ठ है, शास्त्रसम्मत है, उस अनुसार कर्म करता है, चाहे इसके प्रतिफल में उसे स्वयं कुछ भी न प्राप्त हो, तो यह सात्त्विक यज्ञ होता है। परंतु इन सबसे भी आगे जब व्यक्ति सहज रूप से गुरु-आज्ञा से प्रेरित होकर अनन्य रूप से उसी के अनुसार कर्म करता है, जिसमें कर्म का अन्य कोई हेतु नहीं होता, तब वह निखैगुण्य यज्ञ होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि इस प्रकार व्याख्या किये जाने पर यज्ञ का जो संकीर्ण आनुष्ठानिक अर्थ लिया जाता है वह बिल्कुल बदल जाता है और यज्ञ का विधान एक व्यापक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप ग्रहण कर लेता है।
इसी प्रकार तप से भी सामान्यतः जिन तपश्चर्यात्मक क्रियाओं से अर्थ लगाया जाता है केवल वही न होकर इसका गहन मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। तप का अर्थ है अपनी शक्तियों तथा ऊर्जाओं को एकाग्र करना, उन्हें संकेंद्रित करना। किसी छोटे से छोटे कार्य के लिए भी हमें कुछ ऊर्जा को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति जितना ही अधिक अपनी शक्तियों को एकाग्र करने में सफल होता है उतना ही महत् कार्य वह अपने जीवन में संसिद्ध कर पाता है। विश्व में जिन्होंने भी महान उपलब्धियाँ की हैं वे ऐसे लोग रहे जिनमें अपनी शक्तियों को अपने उद्देश्य पर केंद्रित करने की विलक्षण क्षमता रही है। अपनी शक्तियों को जिस उद्देश्य के प्रति हम एकाग्र करते हैं उस अनुसार वह तप तामसिक, राजसिक और सात्त्विक होता है। अतः यह इस पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं को किन हेतुओं की पूर्ति के लिए एकाग्र करता है। यदि किन्हीं निम्न भौतिक हेतुओं की पूर्ति के लिए वह अपनी शक्तियों को एकाग्र करता है तो वह तामसिक तप होगा, यदि किन्हीं प्राणिक कामनाओं, लालसाओं या अन्य अहंपरक आवेगों को पूर्ति के लिए एकाग्र करता है तो वह राजसिक तप होगा और यदि किन्हीं आदर्शों के प्रति, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के प्रति, किसी मानसिक विचार के प्रति वह अपनी शक्तियों का केन्द्रीकरण करता है तो वह सात्त्विक तप होगा। इसी प्रकार जब भगवद्प्रेरणा से प्रेरित होकर सहज रूप से वह अपनी अंतःप्रेरणा के अनुसार अपनी शक्तियों को अर्पित करता है और उसमें किसी प्रकार की कोई अहंपरक तुष्टियों की पूर्ति नहीं खोजता तब इसे निस्त्रैगुण्य तप कहते हैं।
यही बात दान के विषय में भी लागू होती है। अपनी शक्ति या ऊर्जा को एकाग्र कर के जब हम उसे कर्म में नियोजित करते हैं तब उसे दान कहते हैं। किसी भी हेतु की पूर्ति के लिए हमें कुछ न कुछ व्यय अवश्य करना होता है। वह व्यय द्रव्यात्मक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, विचारात्मक या मनोवैज्ञानिक या फिर अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। अतः किन्हीं निम्न हेतुओं के लिए अपनी शक्ति व्यय करना तामसिक दान होता है। जब हम प्राणिक तुष्टियों के लिए जिस किसी भी रूप में शक्ति व्यय करते हैं तब वह राजसिक दान होता है, वहीं किसी प्रतिफल की आशा के बिना जब हम किसी आदर्श के लिए अपनी ऊर्जा या कोई द्रव्य या अन्य कुछ व्यय करते हैं तब उसे सात्विक दान कहते हैं। इसमें व्यक्ति उस कर्म के परिणामों से सरोकार नहीं रखता चाहे है उसके लिए सुखद हों या दुःखद, लाभदायक हों या हानिकारक, शुभ हो या अशुभ। वह तो इसलिए उस कर्म को करता है क्योंकि उसे वह करना उचित लगता है। हालाँकि गीता में यज्ञ, तप और दान का विधान केवल त्रिगुणमय ही बताया गया है, परंतु अपनी टीका में श्रीअरविन्द अपने अनुभव के आधार पर इनमें निखैगुण्य के विधान को भी समाहित कर लेते हैं। आगे भी इस विषय पर गीता में विशद चर्चा आएगी।
इस प्रकार इन तीन तरीकों से श्रद्धा अपने आप को अभिव्यक्त करती है। और प्रत्येक के गठन के अनुसार सभी में यह अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न होगी। साथ ही यज्ञ, तप और दान के इस व्यापक अर्थ से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल कोई बाहरी या आनुष्ठानिक क्रियाएँ ही नहीं हैं, जैसा कि प्रायः ही इन्हें समझा जाता है, अपितु ये तो हमारी सत्ता के वे मूलभूत सत्य हैं जो सभी के ऊपर लागू होते हैं जिनसे कोई भी छूट नहीं सकता। परंतु यदि अवश रूप से ही व्यक्ति इन्हें करता है तो उसे इनका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त होता, वहीं यदि सचेतन रूप से वह इन्हें करता है तो इससे वह अपने सच्चे स्वरूप की ओर उत्तरोत्तर गति करता जाता है और साथ ही सचेतन रूप से करने पर यह एक बहुत ही आनन्ददायक क्रिया बन जाती है। इसीलिए गीता की प्रस्तावना में ही श्रीअरविन्द यह स्पष्ट कर देते हैं कि गीता की शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है जो तत्कालीन आर्य जाति के लिए ही लागू होता हो और जिसका वर्तमान समय में कोई महत्त्व न रह गया हो। गीता के जो विषय हमें देश-काल मर्यादित भी प्रतीत होते हैं, जैसे कि चातुर्वर्ण्य, यज्ञ-तप-दान आदि, यदि उन्हें उनके सही मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक अर्थों में लिया जाए तो वे एक व्यापक और सनातन स्वरूप अपना लेते हैं जो सभी समयों और स्थानों में समान ही रूप से प्रयोजनीय रहते हैं।
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः ।। ३।।
३. हे भारत! प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसकी सत्ता के उपादान द्वारा प्रदत्त रूप ग्रहण कर लेती है। यह पुरुष, मनुष्यगत यह जीव, श्रद्धा का बना हुआ है; और वह श्रद्धा उसके भीतर जो भी है, वह मनुष्य वही है, और वही वह है।
....एक अद्भुत पंक्ति जिसमें गीता हमें बताती है कि यह पुरुष, मनुष्य के अंदर विद्यमान यह जीव, मानो श्रद्धा का, अर्थात् संभूति के संकल्प, अपने-आप में तथा जगत् की सत्ता में विश्वास का बना हुआ है, और उसके अंदर का वह संकल्प, वह श्रद्धा या संघटक विश्वास कोई भी क्यों न हो, वह वही है और वही वह है, 'श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः।' यदि हम इस अर्थगर्भित उक्ति पर कुछ सूक्ष्मता से विचार करें तो हम पाएँगे कि यह एक ही पंक्ति अपने गिने-चुने बलपूर्ण शब्दों में आधुनिक उपयोगितावाद के सिद्धांत की प्रायः सारी ही परिकल्पना को अंतर्निहित रखती है। क्योंकि यदि मनुष्य या उसकी अंतरात्मा अपनी अंतरस्थ श्रद्धा से बनी हई है (श्रद्धा यहाँ अपने सत्य के दर्शन करता है और जिसे जीने का संकल्प करता है, उसके लिए बही सत्तकी सत्ता का, उसके निज स्वरूप का सत्य है जिसकी सृष्टि उसी ने की है या कर रहा है और उसके लिए उसके अतिरिक्त और कोई यथार्थ सत्य नही। हो सकता। यह सत्य उसके आंतर और बाह्य कर्म का तथ्य है, उसकी का, अंतरात्मा की क्रियाशक्ति का तथ्य है, उसके अंदर जो वस्तु नित्य अपरिवर्तनीय है उसका तथ्य नहीं। वह आज जो कुछ भी है वह उसकी अपनी प्रकृति के किसी अतीत संकल्प के द्वारा ही गठित हुआ है। इस समय उसके अंदर कुछ जानने, विश्वास करने तथा अपनी बुद्धि और प्राणशक्ति में वही कुछ बन जाने का जो संकल्प है वह उसके अतीत संकल्प को संपुर करता तथा चालू रखता है। उसकी मूल सत्ता तक में यह जो संकल्प और श्रद्धा क्रियाशील है वह कोई भी नया रूप क्यों न ग्रहण करे, वह भविष्य में उसी नये रूप में परिणत होता जाएगा। हम मन और प्राण के अपने निज कर्म में सत्ता के एक अपने ही सत्य की सृष्टि करते हैं, यह इस बात को कहने का एक दूसरा ढंग है कि हम स्वयं ही अपने स्वरूप की सृष्टि करते हैं, हम स्वयं हो अपने निर्माता हैं।
व्यक्ति की जो भी श्रद्धा होती है वही वह बन सकता है। यदि ऐसा न होता तब तो आध्यात्मिक पथ पर चलने का कोई आधार ही नहीं रहता। जब कोई योग पथ पर आता है तब ऐसा वह केवल श्रद्धा के सहारे ही कर सकता है क्योंकि इसका अन्य कोई प्रमाण तो होता ही नहीं। केवल श्रद्धा ही है जो किसी भी बाहरी प्रमाण के अभाव में भी व्यक्ति को अपने उद्देश्य की दिशा में सतत् लगाए रखती है। इसलिए चाहे बाहरी प्रतीति कुछ भी क्यों न हो, चाहे मन में कितने भी संदेह क्यों न उठते हों, फिर भी भीतर कोई ऐसी चीज होती है जो जानती है कि उसे अमुक काम करना है, या अमुक अभियान पर निकलना है और श्रद्धा के कारण हो सब कुछ के बावजूद वह अपने लक्ष्य को प्रास करता है। अतः गीता का यह एक मूलभूत सत्य है कि व्यक्ति की जो भी श्रद्धा है वैसा वह निश्चित रूप से बन सकता है। और यह तथ्य व्यक्ति को वह शक्ति प्रदान कर देता है जो उसे ब्रह्माण्ड के सभी नियम-विधानों को अतिक्रम करने में सक्षम बना देती है क्योंकि तब सारा खेल तो श्रद्धा का ही रह जाता है। श्रद्धा के विरुद्ध कोई ऊँचे से ऊँचा विधान भी निष्फल हो जाता है। इसका अपना ही अद्भुत विधान होता है। गीता के अनुसार वर्तमान में व्यक्ति जो कुछ भी है वह उसकी अतीत श्रद्धा का परिणाम है, और भविष्य में वह जो कुछ भी होगा वह उसकी वर्तमान श्रद्धा का परिणाम होगा। वास्तव में तो श्रद्धा के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति मनुष्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं हो सकती। यदि ऐसा न होता तब तो साधना या आध्यात्मिक उपलब्धि संभव ही नहीं होते क्योंकि हमारी सतही सत्ता के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिसकी सहायता से वह अपने-आप को अतिक्रम कर सके। और जिस भागवत् उपलब्धि की या साक्षात्कार की हम बात करते हैं, या फिर जिन निर्वाण आदि स्थितियों की बात करते हैं, वे भी किन्हीं बाहरी साधनों से उपलब्ध नहीं हो सकीं। और ये सारी ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ हैं जिनके विषय में व्यक्ति को आरंभ में ही कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए आरंभ करने का तो व्यक्ति के पास कोई आधार ही नहीं होता। बाहरी दृष्टिकोण से तो अवश्य ही यह एक बिल्कुल असंगत बात होती है कि व्यक्ति किसी ऐसी चीज के लिए अपने जीवन को दाँव पर लगा देता है जिसके विषय में वह कुछ भी नहीं जानता। परंतु श्रद्धा का विधान ही सर्वथा भिन्न प्रकार का होता है। इसके विषय में योगी श्रीकृष्णप्रेम कहते हैं, "... आध्यात्मिक अर्थ में श्रद्धा कोई मानसिक विश्वास नहीं है जो विचलित हो सके और बदल सके। मन में यह ऐसा रूप ले सकती है, पर वह विश्वास स्वयं श्रद्धा नहीं है, वह तो उसका केवल बाहरी रूप है। ठीक वैसे ही जैसे देह, बाहरी आकृति तो बदल सकती है पर आत्मा वही बनी रहती है, वैसी ही बात यहाँ भी है। श्रद्धा अन्तरात्मा में विद्यमान एक निश्चयता है जो तर्क-बुद्धि पर, किसी एक या दूसरे मानसिक विचार पर, परिस्थितियों पर, मन या प्राण या शरीर की किसी एक या दूसरी क्षणिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती। यह प्रच्छन्न, अंधकारग्रस्त या आच्छादित, यहाँ तक कि बुझ चुकी या नष्ट हो चुकी भी प्रतीत हो सकती है, परंतु अंधकार का तूफान निकल जाने पर यह पुनः उभर कर आती है; अब भी यह आत्मा में प्रज्ज्वलित गोचर होती है जबकि व्यक्ति ने सोचा था कि यह सदा के लिए बुझाई जा चुकी है। मन अस्थिर संदेहों का समुद्र हो सकता है और तब भी वह श्रद्धा भीतर में हो सकती है, और यदि ऐसा है, तो वह संदेह-प्रताड़ित मन को भी मार्ग में लगाए रखेगी ताकि वह भी अपने स्वभाव के बावजूद अपने नियत लक्ष्य की ओर चलता रहे। श्रद्धा अध्यात्म सत्ता की, भगवान् की तथा आत्मा के आदर्श की एक आध् यात्मिक निश्चिति है, ऐसी कुछ जो उस आदर्श से तब भी चिपकी रहती है जब वह जीवन में चरितार्थ न हो रहा हो, तब भी जब प्रत्यक्ष तथ्य अथवा कठोर परिस्थितियाँ उसका निषेध करती, उसे गलत ठहराती प्रतीत होती हैं। मनुष्य के जीवन में यह एक सामान्य अनुभव है; यदि ऐसा न होता, तो मनुष्य अस्थिर मन का एक खिलौना अथवा परिस्थितियों की कठपुतली-मात्र होता।" (योगी श्रीकृष्णप्रेम, पृष्ठ ३७-३८)
हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि जब हम कहते हैं कि मनुष्य वही बन जाता है जो उसकी श्रद्धा होती है तो यह उसकी संभूति का सत्य होता है। यह हमारे शाश्वत सत्य के विषय में नहीं होता क्योंकि वह तो हमारी सत्ता के द्वारा पूर्णतः अभिव्यक्त हो ही नहीं पाता, उसकी तो केवल आंशिक अभिव्यक्ति ही हो पाती है। वास्तव में श्रद्धा गहरे अर्थ में हमारे अंदर श्रीमाँ का वह निहित विशिष्ट संकल्प है जो हमारी सत्ता के द्वारा अभिव्यक्त होना चाहता है और चूंकि वह स्वयं श्रीमाँ का संकल्प है इसलिए वह अमोघ है। और क्योंकि हम उस संकल्प के विषय में सचेतन नहीं होते इसलिए वह श्रद्धा के रूप में आता है। यह सारा जगत् हमें जैसा दिखाई देता है वैसा वह हमारी श्रद्धा के कारण ही दिखाई देता है। यदि हमारी श्रद्धा बदल जाती है तो हमारी चेतना के लिए सारा दृश्य भी बदल जाएगा। इस अर्थ में श्रद्धा सर्वशक्तिशालिनी है। व्यक्ति इसके आधार पर सब कुछ का निर्माण कर सकता है।
परंतु बिल्कुल स्पष्टतः ही यह सत्य का केवल एक पहलू है, और सभी एक पक्षीय उक्तियाँ विचारक के लिए संदेहास्पद होती हैं। हमारा अपना व्यक्तित्व जो कुछ है या जिस भी चीज की यह सृष्टि करता है, केवल वही सत्य नहीं है; वह सब तो केवल हमारी संभूति का सत्य है, एक विस्तृततम गति के अंदर केवल किसी एक बिंदुविशेष या रेखा पर दिया गया बल है। हमारे व्यक्तित्व के परे, सर्वप्रथम एक विश्वव्यापी सत्ता तथा एक विश्वव्यापी संभूति है, जिसकी हमारी सत्ता और संभूति एक क्षुद्र गति मात्र है; और उसके भी परे है सनातन सत्ता जिसमें से यह समस्त संभूति या भूतभाव उत्पन्न होता है और जो इसकी संभाव्य शक्तियों, इसके तत्त्वों, मूल प्रेरक भावों और चरम उद्देश्यों का स्रोत है।... (पुरुष) एक ही समय में ये सभी चीजें हो सकता है, अर्थात् एक ऐसी सनातन आत्मा हो सकता है जो विश्व में विराट् स्वरूप तथा उसके प्राणियों में व्यष्टिगत रूप धारण किये है; इसी प्रकार वह इन तीनों रूपों में से किसी एक में अपनी चेतना को स्थापित करके प्रकृति की क्रिया को अस्वीकार कर सकता है अथवा इसे अपने नियन्त्रण में रख सकता है या इसके प्रति प्रतिक्रिया कर सकता है, उस एक भाव के अतिरिक्त अन्य दोनों रूपों या भावों को उसके पीछे या उससे दूर रख सकता है, अपने-आप को शुद्ध सनातन सत्ता, आत्मधारक विराट् सत्ता या एकांगी व्यक्तिगत सत्ता के रूप में जान सकता है। इसकी प्रकृति का जो भी बाह्य स्वरूप हो, पुरुष वही बनता प्रतीत हो सकता है और अपनी चेतना के सम्मुखीन सक्रिय भाग में अपने आप को उसी रूप में देखता प्रतीत होता है; परंतु वह कभी भी केवल जितना दिखायी देता है उतना ही सब कुछ नहीं होता; इसके अतिरिक्त वह उतना और भी बहुत कुछ होता है जो कुछ वह बन सकता है; गुप्त रूप में, इसका जो भी अंश अभी तक छुपा हुआ है, यह वह सब ही है। वह काल में होनेवाले अपने किसी भी विशेष आत्म-रूपायन के द्वारा अटल रूप में सीमित नहीं हो जाता, अपितु उसे भेदकर उससे परे जा सकता है, उसे छिन्न-भिन्न कर सकता है या विकसित कर सकता है, अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप-रचना का चुनाव या परित्याग या नव-निर्माण कर सकता है, अथवा अपने अन्दर से किसी महत्तर आत्म-रूपायन को प्रकट भी कर सकता है। अपने उपकरणों में अपनी चेतना के सम्पूर्ण सक्रिय संकल्प के द्वारा यह अपने-आप को जो मानता है या जो विश्वास रखता है वही यह होता है या वही यह बनता चला जाता है, यो यच्छूद्धः स एव सः, अर्थात् जो कुछ बन सकने में वह विश्वास रखता है तथा जैसा बन सकने में इसकी पूर्ण श्रद्धा होती है, इसकी प्रकृति उसी में बदलती जाती है, यह उसी को विकसित या उपलब्ध करता है।
पुरुष (अंतरात्मा) का अपनी प्रकृति के ऊपर यह अधिकार आत्मसिद्धियोग में चरम महत्त्व रखता है; यदि यह न होता तो हम सचेतन प्रयत्न और अभीप्सा के द्वारा अपने वर्तमान अपूर्ण मानव-जीवन के नियत या निर्धारित चक्र में से कभी नहीं निकल सकते थे; (उस स्थिति में) यदि कोई महत्तर पूर्णता हमारे लिये अभिप्रेत होती तो हमें प्रतीक्षा करनी होती कि प्रकृति विकास की अपनी मन्द या तीव्र प्रक्रिया के द्वारा उसे साधित करे।
इसमें एक नया तत्त्व यह जुड़ गया है कि हमारी सत्ता का एक व्यष्टिगत पक्ष होने के साथ ही साथ समष्टिगत पहलू भी है। यही नहीं, व्यष्टि और समष्टि से परे हमारी सत्ता का परात्पर पहलू भी है। इसलिए हमारी श्रद्धा भी केवल व्यष्टिगत ही नहीं होती। अतः यह संभव है कि हमारी समष्टिगत चेतना की महत्तर श्रद्धा की चरितार्थता के लिए व्यष्टिगत श्रद्धा की चरितार्थता को प्रतीक्षा करनी पड़े। साथ ही यह संभावना भी रहती है कि व्यक्ति अपनी चेतना में अपने परात्पर पहलू की श्रद्धा को भी सक्रिय कर सके। इसी अर्थ में कह सकते हैं कि अपनी पूर्ण सत्ता में व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता है ही नहीं और सारी अभिव्यक्ति केवल उसी का भीतर से प्रक्षेपण है। इसलिए किसी चरम अर्थ में यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह व्यष्टिभावापन्न अहमात्मक चेतना में बने रहना चाहता है या फिर अपनी वैश्विक सत्ता की चेतना में निवास करना चाहता है या फिर इन सबसे परे की चेतना में निवास करना चाहता है या फिर एक ही साथ तीनों चेतनाओं में निवास करना चाहता है। यदि ऐसा न होता तब तो व्यक्ति अवश रूप से प्रकृति के विधान से बाध्य होता और जिस मंद गति से वह विकास करती है उसे उसी का अनुसरण करना होता। ऐसे में तो किसी प्रकार की आध्यात्मिक साधना या चेतना में सचेतन आरोहण की तो कोई संभावना ही नहीं होती। परंतु ऐसा नहीं है। व्यक्ति सच्चे अर्थों में पूर्णतः स्वतंत्र है और जैसी उसमें श्रद्धा होगी वैसा वह निश्चित ही बन सकता है। यह एक बड़ा ही रहस्यमय और गुह्य सत्य है जो हमें प्रतीत होती अंध नियति से छुटकारा प्रदान कर परम आशा से भर देता है। वर्तमान में यदि व्यक्ति बाह्य प्रकृति से इतना वशीभूत और बाध्य प्रतीत होता है तो इसका कारण भी यही है कि आत्मा ने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं सचेतन रूप से अपने ऊपर इन परिस्थितियों को लादा है। यदि उसका चयन इससे भिन्न होता तो उसी के अनुसार बाहरी परिस्थितियाँ भी भिन्न होतीं। इसी अर्थ में गीता का यह वचन सर्वथा निरपेक्ष प्रकार का है कि 'यो यच्छूद्धः स एव सः'।
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।
प्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ।। ४।।
४. सात्त्विक मनुष्य देवताओं को यज्ञ समर्पित करते हैं, राजसिक मनुष्य यक्षों और राक्षसों को, और दूसरे, तामसिक मनुष्य प्रेतों और भूतों को यज्ञ अर्पित करते हैं।
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ।। ५।।
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्वयान् ।। ६।।
५-६. दम्भ और अहंकार से ग्रसित, कामनाओं और आवेगों के बल द्वारा माहीत, जो मनुष्य अशाखसम्मत भीषण तप करते हैं, स्थूल शरीर के जाभूत पंचभूतों को और शरीर में निवास करनेवाले मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं। उन संज्ञाहीन अविवेकी जनों को आसुरी निश्चयों या संकल्पों वाला जान।
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ।। ७।।
७. जो भोजन प्रत्येक को प्रिय होता है वह भी त्रिविध स्वरूप का होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी (तीन-तीन प्रकार के होते हैं), उनके इस भेद को सुन।
समस्त स्फूर्त-गतिशील क्रिया को मूलतः इन तीन अंगों में विश्लेषित किया जा सकता है। क्योंकि समस्त शक्तिशाली क्रिया में, प्रकृति की समस्त गतिशीलता के अंदर एक ऐच्छिक या अनैच्छिक तपस्या निहित रहती है, हमारी शक्तियों या क्षमताओं की या किसी एक क्षमता की तेजस्विता और एकाग्रता रहती है जो हमें कुछ उपलब्ध या अर्जित करने या कुछ बनने में सहायता देती है, वही तपस् है। समस्त क्रिया में, जो कुछ हम हैं या जो कुछ हमारे पास है उसका दान अर्थात् एक प्रकार का व्यय निहित रहता है जो उस उपलब्धि का, उस अर्जन या संभूति का मूल्य होता है, वही दान है। समस्त क्रिया में अधिभौतिक शक्तियों या विश्वशक्तियों के प्रति या हमारे कर्मों के परम प्रभु के प्रति एक यज्ञ भी निहित होता है। प्रश्न यह है कि क्या हम ये कार्य अचेतन एवं निष्क्रिय रूप से करते हैं, अथवा अधिक-से-अधिक एक बुद्धिहीन, अज्ञ, अर्धचेतन संकल्प के साथ, या एक ऐसी शक्ति या ऊर्जस्विता के साथ करते हैं जो अज्ञानयुक्त या विकृत रूप से चेतन होती है या एक ऐसे संकल्प के साथ जो विज्ञ रूप से चेतन तथा ज्ञान पर सुप्रतिष्ठित होता है, दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह है कि क्या हमारे यज्ञ, दान और तप तामसिक प्रकृति के हैं या राजसिक या सात्त्विक प्रकृति के।
क्योंकि, यहाँ की सभी वस्तुएँ, भौतिक वस्तुओं समेत, इसी त्रिविध स्वरूप की हैं। उदाहरणार्थ, गीता हमें बताती है कि हमारा भोजन अपने गुण के अनुसार तथा शरीर पर होनेवाले अपने प्रभाव के अनुसार सात्त्विक, राजसिक या तामसिक होता है।
गीता यहाँ कहती है कि 'सात्त्विक मनुष्य देवताओं को यज्ञ समर्पित करते हैं, राजसिक मनुष्य यक्षों और राक्षसों को, और दूसरे, तामसिक मनुष्य प्रेतों और भूतों को यज्ञ अर्पित करते हैं।' यदि हम इसे भौतिक अर्थ में लें तो यह समझना कठिन है कि किस प्रकार व्यक्ति देवताओं को या फिर भूतों, प्रेतों या राक्षसों को यज्ञ अर्पित करता है। कुछ लोग इससे किन्हीं तंत्र पद्धतियों की साधना, अघोर साधना आदि का अर्थ लगाते हैं। परंतु यदि गीता का अर्थ ऐसी किन्हीं संकीर्ण साधना पद्धतियों से होता तब तो यज्ञ विधान आज के समय में अब और अधिक प्रासंगिक नहीं रहता जबकि गीता तो यहाँ ऐसे किसी भी देश-काल से सीमित तत्त्व की चर्चा नहीं कर रही है। वह जिस यज्ञ-विधान की चर्चा करती है वह तो सभी समयों में और सभी पर समान ही रूप से लागू होता है। तब फिर आखिर भूतों, प्रेतों, राक्षसों, देवताओं आदि को यज्ञ अर्पित करने का अर्थ क्या है? वस्तुतः, जो तामसिक वृत्ति वाले लोग हैं वे अधिकाधिक केवल ग्रहण करना चाहते हैं, बदले में कुछ देना नहीं चाहते। इसे ही भूतों और प्रेतों को यज्ञ समर्पित करना कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तामसिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति के मन, प्राण और शरीर में भूतों-प्रेतों का वास होता है और वे ही मनुष्य की सत्ता को अधिकृत कर के उसके द्वारा अपनी क्रिया करते हैं। इससे आगे जब व्यक्ति केवल अपने आप के विषय में ही न सोचकर दूसरों के विषय में भी सोचता है और यह जानता है कि सामूहिक जीवन में वह यदि दूसरों के प्रति कुछ करेगा तभी प्रतिफल में दूसरे भी उसे समय पर सहायता करेंगे। इसे राजसिक यज्ञ कहते हैं जिसमें व्यक्ति यक्षों और गंधर्वो को यज्ञ अर्पित करता है। राजसिक व्यक्ति की सत्ता यक्ष, गंधर्व आदि सत्ताओं के अधिकार में होती है और वे ही उसके माध्यम से काम करते हैं और अपने हेतुओं को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।
सात्त्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करता है। देवताओं की पूजा करने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी भौतिक और प्राणिक प्रकृति से ग्रसित न होकर उचित तथा श्रेष्ठ का विचार कर के कार्य करता है। इसमें व्यक्ति को प्रतिफल की आशा नहीं रहती और न ही अपने कार्य के परिणाम की कोई चिंता होती है। अपने कार्य के परिणाम के रूप में उसे सुख हो या दुःख, लाभ हो या हानि, वह इन सबको अनदेखा कर के जो करने योग्य है इसका विचार कर के कर्म करता है।
सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति में सच्चाई, सद्भावना, संतोष, प्रेम, सामंजस्य आदि गुण देखने को मिलते हैं जिसमें दैवी प्रकृति का प्रभाव रहता है। अब व्यक्ति सात्विकता में और आगे बढ़ता है तब उसके अंदर भगवान् की पूजा, देवताओं के प्रति आस्था, भगवान् के प्रति समर्पण भाव आदि गुण दिखाई देते हैं। परंतु श्रीअरविन्द के अनुसार सात्विक भाव में भी व्यक्ति त्रिगुणों से परे नहीं जा सकता। वह रहता त्रिगुणों के बंधन में ही है। श्रीरामकृष्ण परमहंस का भी यही कहना था कि ये तीनों गुण उन तीन जंजीरों के समान हैं जिनमें तामसिक गुण लोहे की, राजसिक गुण चाँदी की और सात्विक गुण सोने की जंजीर के समान है, परंतु हैं सभी जंजीरें ही जिनमें कि मनुष्य बंध जाता है। इन सब स्थितियों से ऊपर की स्थिति वह है जब व्यक्ति स्वयं को जगदम्बा के हाथों में सौंप देता है और केवल उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार क्रिया करता है। यह त्रिगुणों से परे निस्त्रैगुण्य की स्थिति की ओर अग्रसर होना है जिसमें व्यक्ति जितना ही अधिक पूर्ण रूप से अपने आप को जगज्जननी जगदंबा के हाथों में देता है उतना ही अधिक गुणों की क्रिया से मुक्त होता जाता है। यह व्यक्ति को मनुष्यता की सीमाओं से ऊपर उठा देता है। श्रीअरविन्द के अनुसार देवताओं आदि की पूजा करना भूतों, प्रेतों आदि की पूजा करने से तो बहुत अधिक श्रेष्ठ है परन्तु वास्तव में श्रीमाताजी को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना ही एकमात्र सच्चा कार्य है। वस्तुतः यह समर्पण अंतरात्मा की सहज पुकार होती है क्योंकि पराप्रकृति स्वयं ही जीव बनती हैं इसलिए अपने निज स्वरूप के प्रति पुकार या आकर्षण होना आत्मा का सहज स्वभाव है। और जब व्यक्ति अपने आप को श्रीमाताजी के हाथों में सौंप देता है तब जो भी कार्य वह करता है वह उन्हीं की अभिव्यक्ति होने के कारण श्रेष्ठतम ही होगा। उस भाव में किन्हीं निम्न चीजों के प्रवेश की कोई संभावना नहीं होती। हालाँकि गीता इस स्थिति का वर्णन नहीं करती परंतु श्रीअरविन्द अपने अनुभव के आधार पर इसका निरूपण करते हैं।
यज्ञ के बाद गीता तप की चर्चा करती है। हमारे पुराणों में वर्णित कथाओं में हम प्रायः ही पाते हैं कि अधिकांशतः जितना कठोर तप दैत्य, असुर, राक्षस आदि करते हैं मनुष्य तो कदाचित् ही उतने कठिन तप कर पाते हों। हिरण्यकशिपु, रावण आदि द्वारा किये जिस प्रकार के भीषण तपों का हम वर्णन पाते हैं वे तो किसी सामान्य मनुष्य की कल्पना से भी सर्वथा परे हैं। अपनी आसुरी वृत्ति के प्रभाव से उनके अंदर कुछ प्राप्त करने की अत्यंत प्रबल इच्छा होती है जिसके कारण वे ऐसे कठोर तप करते हैं। इसीलिये छठे श्लोक में भगवान् कहते हैं कि 'दम्म और अहंकार से ग्रसित, कामनाओं और आवेगों के बल द्वारा चालित, जो मनुष्य अशास्त्रसम्मत भीषण तप करते हैं, स्थूल शरीर के अंगभूत पंचभूतों को और शरीर में निवास करनेवाले मुझे भी कष्ट पहुँचाते हैं; उन संज्ञाहीन अविवेकी जनों को आसुरी निश्चयों या संकल्पों वाला जान।' इस प्रकार का तप आसुरी प्रकार का होता है। यह तो तप का चरम रूप है। परंतु वास्तव में तप का अर्थ है अपनी शक्तियों और ऊर्जाओं को किसी हेतु के लिए एकाग्र करना। कोई भी काम करने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ शक्ति एकाग्र करनी ही होती है। कोई भौतिक क्रिया को करने के लिए भी व्यक्ति को उसमें ध्यान देना पड़ता है। भोजन पकाने, बाजार से सामान लाने आदि जैसी दैनंदिन क्रियाओं को भी सही रूप से करने के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति को परीक्षा उत्तीर्ण करनी हो तो उसके लिए भी उसे वहाँ किसी हद तक अपनी इंद्रियों आदि को संयमित करके अपने ऊपर कुछ अनुशासन लागू करना होता है, प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अनुशासित जीवन जीने के लिए भी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर कुछ हद तक नियंत्रण करना होता है अन्यथा तो सामान्य जीवन भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अतः मूलतः तो किसी भी चीज के लिए व्यक्ति को अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा को एकाग्र करना होता है। परंतु जब सामान्य से कुछ अधिक मात्रा में अपनी ऊर्जाओं को एकाग्र करना होता है तब हम उसे तप की संज्ञा दे देते हैं। गीता के अनुसार तप भी तीन प्रकार का होता है - सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह कर्म के हेतु पर निर्भर करता है कि वह तप तामसिक होगा या राजसिक या फिर सात्त्विक। यही बात दान के लिए भी लागू होती है।
प्रश्न : अशास्त्रसम्मत भीषण तप का क्या अर्थ है?
उत्तर : शास्त्रसम्मत तप में शास्त्र द्वारा निर्धारित मानक या मापदंड होते हैं। उदाहरण के लिए संगीत, नृत्य आदि सभी कलाओं का अपना-अपना विधिवत् शास्त्र होता है जिसकी मर्यादाओं का पालन करना होता है तभी वह प्रामाणिक और शास्त्रसम्मत होता है अन्यथा तो उसे त्रुटिपूर्ण ही माना जाता है। शास्त्र का अर्थ है सुदीर्घ अनुभव द्वारा सिद्ध और प्रामाणित विधान जिनका पालन करने पर ही सर्वोत्तम परिणाम प्रास हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भोजन पकाने की भी अपनी एक तय प्रक्रिया है। उसका सही अनुसरण कर के ही व्यक्ति सही भोजन पका सकता है। यदि इसमें वह मनमौज के अनुसार चले तो कदाचित् ही अच्छा भोजन पका पाएगा। इसी प्रकार सभी चीजों के प्रयोग या अनुभव-सिद्ध विधि-विधान होते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे अपने दंभ और अहंकार तथा कामनाओं आदि से ग्रसित होकर शास्त्र की अवहेलना कर के अपने शरीर आदि भागों को कष्ट में डालकर तप करते हैं। ऐसे तप को अशास्त्रसम्मत कहते हैं।
प्रश्न : बहुत से लोग अपने शरीर को बहुत कष्ट देकर तपस्या करते हैं जैसे कि एक पैर पर खड़े रहना, तेज गर्मी में अपने चारों ओर आग का घेरा बनाकर उसके बीच में बैठ जाना आदि-आदि, तो यह भी अशास्त्रसम्मत है?
उत्तर : इसके विषय में श्रीमाताजी जो कहती हैं वह जानकर हमें यह भान हो जाएगा कि वास्तव में यह सब कष्ट देना सही है या नहीं। वे कहती हैं, "...पहले मुझे एक प्रश्न स्पष्ट कर देना चाहिये जो अधिकतर लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियों और उलझनों का कारण है। यह है तपश्चर्यात्मक क्रियाओं के बारे में, जिन्हें लोग आध्यात्मिक साधना समझने की भूल कर बैठते हैं। ये क्रियाएँ, जिनमें शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए कि, आत्मा को उससे मुक्त किया जा सके, वास्तव में आध्यात्मिक साधना की एक ऐंद्रिय विकृति हैं; कष्ट पाने की एक प्रकार की विकृत आवश्यकता ही है जो तपस्वी से आत्म-पीड़न करवाती है। साधु का कीलों के बिछौने पर सोना और ईसाई संन्यासी का कोड़े खाना और टाट की वेशभूषा पहनना न्यूनाधिक रूप से पीड़ा के प्रति आसक्ति को छिपी हुई प्रवृत्ति है जिसे न तो स्वीकार किया जाता है, न स्वीकार करने योग्य ही है। यह उग्र संवेदनों के लिये एक अस्वस्थ चाह या अवचेतन आवश्यकता है। वास्तव में, ये चीजें आध्यात्मिक जीवन से कोसों दूर की हैं क्योंकि ये भदी, निम्नकोटि की, अंधकारपूर्ण और रुग्ण हैं; जबकि इनके विपरीत, आध्यात्मिक जीवन प्रकाश और संतुलन, सौंदर्य और आनंद का जीवन है। उन चीजों का आविष्कार और गुणगान तो शरीर पर की जाने वाली एक प्रकार की मानसिक और प्राणिक क्रूरता द्वारा ही किया जाता है। परंतु चाहे वह अपने शरीर के साथ ही क्यों न हो, पर क्रूरता आखिर क्रूरता ही है, और सभी प्रकार की क्रूरता भारी निश्चेतना का चिह्न है। अचेतन प्रकृतियों को तीव्र संवेदनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके बिना उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता; और क्रूरता, जो कि एक प्रकार की उत्पीड़न की आसक्ति है, बहुत तीव्र संवेदन पैदा करती है। इस प्रकार की क्रियाओं का उद्देश्य यह माना जाता है कि सभी प्रकार के संवेदनों को समाप्त कर दिया जाये ताकि शरीर हमारी आत्मा की ओर की उड़ान में और अधिक बाधा न दे सके; परंतु इस पद्धति की उपयोगिता संदेहास्पद है। यह भली-भाँति जानी हुई बात है कि तेजी से प्रगति करने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिये; इसके विपरीत, प्रत्येक सुअवसर पर कठिन चीज करने का चयन करने से व्यक्ति अपनी संकल्प-शक्ति को बढ़ाता है और स्नायुओं को बलिष्ठ करता है। वास्तव में, तपस्या की विकृतियों और उनके विघटनकारी परिणामों के द्वारा सुख की विकृतियों और उनके अज्ञानमय परिणामों के साथ संघर्ष करने की अपेक्षा, संयम और संतुलन के साथ समुचितता और स्थिरता का जीवन बिताना कहीं अधिक कठिन है। अपनी भौतिक सत्ता के साथ इस हद तक बुरा व्यवहार करना कि वह शून्यवत् हो जाये, इसकी अपेक्षा, उसमें स्थिरता और सरलता के साथ सामंजस्यपूर्ण उत्तरोत्तर विकास कर पाना बहुत अधिक कठिन है। बड़े गर्व के साथ अपने संयम या त्याग का प्रदर्शन करने के लिये शरीर को उसके लिये आवश्यक आहार और शुद्ध अभ्यासों से वंचित करने की अपेक्षा, सौम्य रूप से और कामना के बिना जीना कहीं अधिक कठिन है। रोग या दुर्भावना की अवहेलना करने और उसकी ओर ध्यान न देने और उसे अपना विनाशकार्य करते रहने देने की अपेक्षा, उस पर आंतरिक और बाह्य सामंजस्य, शुद्धि और संतुलन द्वारा विजय प्राप्त करना या रोग को टाल देना बहुत अधिक कठिन है। और सबसे कठिन काम है चेतना को सतत् रूप से उसकी क्षमता के शिखर पर बनाये रखना और शरीर को कभी निम्नतर आवेगों या प्रेरणाओं के प्रभाव में आकर काम न करने देना।" (CWM 12, 49-50)
श्रीमाताजी के वचनों से यह स्पष्ट ही हो जाता है कि वास्तव में तपस्या के ऐसे किन्हीं भी तथाकथित तरीकों का सच्ची आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। श्रीमाताजी व श्रीअरविन्द ने तो अपने योग में सदा ही ऐसी किन्हीं भी चीजों को अपने से दूर रखने पर बल दिया है क्योंकि ये सभी चीजें केवल प्राणिक प्रकृति के तीव्र संवेदनों की तृष्णा की ही पूर्ति करती हैं, अहंकार को बढ़ा देती हैं और भगवद्-विरोधी सत्ताओं को पुष्ट करती हैं तथा साधक के सच्चे संतुलन को सर्वथा बिगाड़ देती हैं।
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८॥
८. जो भोजन जीवन, प्राण-शक्ति, बल, स्वास्थ्य, हर्ष तथा प्रसन्नचित्तता को बढ़ाने वाले हैं, जो रसयुक्त, नर्म (घृतादि स्निग्ध पदार्थयुक्त), पुष्टिकारक अथवा स्थिर रहने वाले (दीर्घकाल तक शरीर में रहने वाले), हृदय को तृप्त करनेवाले हैं, वे सात्त्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं।
कट्द्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।। ९।।
९. जो भोजन कड़वे, खट्टे, (अत्यधिक) नमकवाले, अत्यधिक उष्ण, तीखे, रूखे (जैसे भाड़ में भुने अन्न) और दाहजनक होते हैं तथा जो पीड़ा, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले हैं वे राजसिक मनुष्यों को प्रिय होते हैं।
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ।। १० ।।
१०. जो भोजन बिगड़ गया है, स्वादहीन है, दुर्गंधयुक्त है, पुराना है, दूसरों का जूठा है और जो अपवित्र है, वह तामसिक मनुष्यों को प्रिय होता है।
इन तीन गुणों की क्रिया सर्वव्यापी है। दूसरे छोर पर ये गुण मन और आत्मा की चीजों, यज्ञ, दान और तप, पर भी इसी प्रकार लागू होते हैं: प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीकवाद ने इन तीन चीजों के जिन रूपों की परिकल्पना की थी उन्हीं प्रचलित रूपों के अनुसार गीता इनमें से प्रत्येक के तीन प्रकार के विभाग करती है। परंतु, स्वयं गीता यज्ञ के विचार को जो अत्यंत व्यापक अर्थ प्रदान करती है उसे स्मरण रखते हुए, हम सहज ही इन संकेतों के स्थूल अर्थ को विस्तृत करके इनका एक उदारतर मर्म प्रकाशित कर सकते हैं।
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।। ११ ।।
११. जिस यज्ञ को बिना फल की कामना के, यथार्थ विधि के अनुसार, करने योग्य कर्म को सच्चे यज्ञ के रूप में मानते हुए उसके भाव पर मन को केंद्रित और स्थित करके अनुष्ठान किया जाता है, वह सात्त्विक यज्ञ होता है।
अतः, गीता जिस आदर्श की तथा जिस प्रकार के कर्म की माँग करती है, यह सात्विक यज्ञ उसके अत्यंत निकट है और यह उसकी ओर सीधे ही ले जाता है; परंतु यह कोई चरम और परम आदर्श नहीं है, यह अभी भी उस सिद्ध पुरुष का कर्म नहीं है जो दिव्य प्रकृति में निवास करता है। क्योंकि, यह एक नियत-निर्धारित धर्म के रूप में सम्पन्न किया जाता है, और यह देवताओं के प्रति, हमारे अंदर या विश्व के अंदर अभिव्यक्त भगवान् की किसी आंशिक शक्ति या रूप के प्रति यज्ञ या सेवा के रूप में अर्पित किया जाता है। निःस्वार्थ धार्मिक श्रद्धा-विश्वास के साथ किया गया कर्म या स्वार्थ-रहित भाव से मानवजाति के लिए किया गया कर्म अथवा न्याय या सत्य के प्रति निष्ठा से प्रेरित होकर निर्वैयक्तिक भाव से किया गया कर्म इस सात्त्विक प्रकृति का होता है, और इस प्रकार का कर्म हमारी पूर्णता के लिए आवश्यक है; क्योंकि यह हमारे विचार, संकल्प तथा हमारे प्रकृतिगत उपादान को शुद्ध करता है। परंतु सात्त्विक कर्म की जिस सर्वोच्च परिणति तक हमें पहुँचना है वह और भी व्यापकतर तथा मुक्ततर प्रकार की है; वह एक उच्च कोटि का चरम यज्ञ है जिसे हम पुरुषोत्तम को पाने की अभीप्सा से या सभी कुछ में वासुदेव के दर्शन करते हुए परम और समग्र भगवान् के प्रति निवेदित करते हैं; वह एक ऐसा कर्म है जो निर्वैयक्तिक एवं विश्वगत भाव से, जगत् के मंगल के लिए तथा विश्व में भगवत्संकल्प की परिपूर्ति के निमित्त किया जाता है। वह परिणति फिर अपने से भी परे, अमर धर्म की ओर ले जाती है। क्योंकि तभी एक ऐसी मुक्ति प्राप्त होती है जिसमें लेशमात्र भी कोई वैयक्तिक कर्म, धर्म का कोई सात्त्विक विधान और शास्त्र की कोई बाध्यता नहीं रहती। वहाँ स्वयं निम्न बुद्धि और संकल्प भी अतिक्रांत हो जाते हैं और उनकी जगह एक उच्चतर प्रज्ञा हमारे कर्म को प्रेरित और परिचालित करती है तथा उसके लक्ष्य पर प्रभुत्व रखती है। तब व्यक्तिगत फल का कोई प्रश्न ही नहीं रहता; क्योंकि जो संकल्प कार्य करता है वह हमारा अपना नहीं, अपितु एक परमोच्च संकल्प होता है जिसकी कि हमारी अंतरात्मा एक यंत्र मात्र होती है... तब कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं रहता, क्योंकि सभी कर्म हमारे कर्मों के प्रभु के प्रति उत्सर्ग कर दिये जाते हैं और तब वे ही हैं जो हमारी दिव्यीकृत प्रकृति के द्वारा कर्म करते हैं। वहाँ कोई यज्ञ भी नहीं होता, - हाँ, हम यह अवश्य कह सकते हैं कि यज्ञ के अधीश्वर जीव में विद्यमान अपनी शक्ति के कर्मों को अपनी ही विश्वरूपमय सत्ता के प्रति अर्पित कर रहे होते हैं। यज्ञरूप कर्म के द्वारा आत्म-अतिक्रमण की जो परमोच्च स्थिति मा होहोती है। यह यही है, यही उस जीव की पूर्णावस्था है जो दिव्य प्रकृति में अपनी पूर्ण चेतना लाभ कर लेता है।
गीता सात्त्विक यज्ञ तक ही ठहर जाती है। परंतु श्रीअरविन्द के अनुसार यह दिव्य प्रकृति में निवास करने वाले सिद्ध पुरुष का यज्ञ नहीं होता। श्रीअरविन्द सात्त्विक यज्ञ से भी आगे उस स्थिति तक ले जाते हैं जहाँ व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत संकल्प नहीं रहता। उसका कर्म तब किन्हीं देवताओं के निमित्त नहीं होता अपितु अब उसके कर्म का आरंभ, उत्प्रेरण और नियोजन स्वयं भगवान् की परा प्रकृति या दिव्य प्रकृति करती है जो कि परम् प्रभु से एक होती है। अतः इसमें व्यक्ति के अपने संकल्प-विकल्प आदि का तो कोई स्थान ही नहीं होता। इस प्रकार चेतना की यह स्थिति सात्त्विक यज्ञ से सर्वथा भिन्न प्रकार की होती है।
अभिसंघाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ।। १२ ।।
१२. हे भरतश्रेष्ठ! जो यज्ञ फल को ध्यान में रखते हुए, और दिखावट के लिये भी किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसिक जान।
हमारे कर्मों का मूल्य केवल उनकी प्रतीयमान बाह्य दिशा से ही निर्धारित नहीं होता, न वह उन देवताओं के द्वारा निर्धारित होता है जिनके नाम की दुहाई देकर हम अपने कर्मों का अनुमोदन कर सकते हैं और न ही उस सच्चे बौद्धिक विश्वास के द्वारा जो उनके अनुष्ठान में हमारा समर्थन करता प्रतीत होता है, अपितु वह निर्धारित होता है आंतरिक स्थिति, हेतु और दिशा के द्वारा। जहाँ कहीं हमारे कर्मों में अहंकार की प्रधानता होती है, वहाँ हमारा कर्म राजसिक यज्ञ बन जाता है।
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ।। १३।।
१३. जो यज्ञ उचित विधि के अनुसार अनुष्ठित न हो, अन्नदान से रहित, मन्त्र के बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिये बिना, श्रद्धा से शून्य हो उस यज्ञ को तामसिक कहते हैं।
तामसिक यज्ञ वह कर्म है जो बिना श्रद्धा के किया जाता है, अर्थात् किये जाने वाले कर्म के किसी पूर्ण सचेतन बोध, उसकी स्वीकृति एवं उसके करने के संकल्प के बिना ही किया जाता है जिसे फिर भी प्रकृति हमसे बरबस करवाती है। वह यंत्रवत् किया जाता है, क्योंकि जीवनधारण के लिए उसे करना आवश्यक होता है, क्योंकि वह हमारे सामने आकर उपस्थित हो जाता है, और क्योंकि दूसरे लोग उसे करते हैं, अथवा किसी अन्य बड़ी मुसीबत से बचने के लिए किया जाता है जो उसे न करने से पैदा हो सकती हेतु से किया जाता है। और है. या फिर मारा स्वभाव पूरी तरह से इसी (तामसिक) प्रकार का हो तो यह कर्म भी संभवतः लापरवाही से, उदासीन भाव से यंत्रवत् तथा गलत ढंग से ही किया जाना है। वह विधि के अनुसार अथवा शास्त्र के यथार्थ विधान के अनुसार नहीं किया जाएगा, और उसका गतिक्रम उस यथायथ विधि के अनुसार परिचालित नहीं होगा जो जीवन की कला और विधान के द्वारा तथा करणीय कर्म के सच्चे विज्ञान के द्वारा निर्धारित है। उस यज्ञ में हव्य-दान नहीं होगा, – और भारतीय कर्मकांड में यह क्रिया एक उस सहायक या उपकारी दानतत्त्व का प्रतीक है जो वास्तविक यज्ञ कहलाने वाले प्रत्येक कर्म के अंदर निहित होता है, दूसरों को दिया जानेवाला यह दान एक अनिवार्य वस्तु है, यह दूसरों की एवं जगत् की फलप्रद सहायता है जिसके बिना हमारा कर्म एक सर्वथा स्वार्थपूर्ण वस्तु बन जाता है और वह एकसूत्रता तथा आदान-प्रदान के सच्चे विश्व-विधान का उल्लंघन करने वाला बन जाता है। वह कर्म उस दक्षिणा के बिना ही संपन्न किया जाएगा जो कि यज्ञीय कर्म के पुरोहितों को दिया जाने वाला एक अत्यावश्यक दान या आत्मदान है, भले ही वह दान हमारे कर्म के किसी बाह्य मार्गदर्शक एवं सहायक को दिया जाए या अपने अंदर स्थित प्रच्छन्न या व्यक्त भगवान् को। वह मंत्र के बिना अर्थात् उस समर्पणात्मक विचार के बिना ही किया जाएगा जो कि हमारे उस संकल्प तथा ज्ञान की पावन देह है जो हमारे यज्ञ के उपास्य देवों की ओर ऊपर उठे होते हैं। तामसिक मनुष्य अपना यज्ञ देवताओं को अर्पित नहीं करता, अपितु निम्न आधिभौतिक शक्तियों को या आवरण के पीछे अवस्थित उन स्थूलतर प्रेतात्माओं को अर्पित करता है जो उसके कार्यों के द्वारा अपना भोग-साधन करते हैं तथा उसके जीवन को अपने अंधकार के द्वारा आच्छन्न कर देते हैं।
प्रश्न : बारहवें श्लोक की टीका में श्रीअरविन्द कहते हैं कि, "जहाँ कहीं हमारे कर्मों में अहंकार की प्रधानता होती है, वहाँ हमारा कर्म राजसिक यज्ञ बन जाता है।" अहंकार की प्रधानता तो सभी मनुष्यों में रहती है, तो फिर केवल राजसिक मनुष्यों में ही अहंकार की प्रधानता क्यों बताई गई है?
उत्तर : यों तो अहंकार सत्त्व, रजस् और तमस् तीनों ही गुणों में रहता है परंतु अधिक प्रकट रूप से हमें वह राजसिक प्रवृत्ति में ही दिखाई देता है। तामसिक व्यक्तियों में तो घोर अहंकार होता है, वे केवल अपने ही विषय में सोचते हैं और बिना कुछ व्यय किये केवल ग्रहण ही करना चाहते हैं। परन्तु राजसिक व्यक्ति में इसकी अभिव्यक्ति अधिकतम होती है। राजसिक व्यक्ति प्राण प्रधान होता है जिसमें गतिशील और कर्मप्रधान प्रकृति की प्रधानता रहती है। यहाँ तक कि भौतिक और मानसिक कायर्यों को भी करने के लिए प्राणिक ऊर्जा आवश्यक होती है। इसलिए प्राणप्रधान व्यक्ति में अतिशय रूप से अपनी सत्ता को प्रतिष्ठित करने की, बहुत बड़ा कार्य संसिद्ध करके अपना नाम कमाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसी कारण अहंकार की अधिकतम अभिव्यक्ति राजसिक प्रकृति में होती है। बाकी के दो गुणों में अहं तो होता है परंतु उसमें किसी महत् उपलब्धि से मिलने वाली तुष्टि और उससे परिवर्धित होने वाला अभिमान या घमंड नहीं होता। केवल राजसिक व्यक्ति ही है जो भीषण कर्म करने से भी नहीं चूकता यदि उससे उसके अहं की तुष्टि होती हो और लोग स्वीकार करते हों कि उसने बहुत ही भीषण और अद्वितीय कर्म किया है।
गीता तीन प्रकार के सात्त्विक तपों का निरूपण करती है।
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ।। १४।।
१४. देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी की पूजा करना, शुचिता, स्पष्टवादिता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का पालन करना, इन्हें शारीरिक तप कहा जाता है।
जिस प्रचलित अर्थ में हम इस तप शब्द को लेते हैं गीता की परिभाषा का उससे कोई संबंध नहीं है। प्रचलित तौर पर तप शब्द से हम शारीरिक उत्पीड़न का अर्थ लगाते हैं परंतु गीता का तप ऐसा नहीं है हालाँकि जिस तप की गीता बात करती है वह तो किन्हीं भी भीषण से भीषण शारीरिक उत्पीड़नों से भी कहीं अधिक कठिन है। शरीर को कष्ट देने से तो व्यक्ति का अहं अत्यधिक पुष्ट होता है और फूल उठता है। परंतु गीता के तप का पालन करने में तो प्राण का भी संयमन हो जाता है इसलिए यही वास्तविक तप है। इसमें किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं है, किसी प्रकार की कोई अस्वास्थ्यकर चीज नहीं है अपितु यह तो अपने आप पर अनुशासन लागू करके अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करना और ऊर्ध्वमुखी विकास करना है जबकि शरीर को यंत्रणा देकर किसी प्रकार का कोई सच्चा विकास नहीं होता अपितु यह तो एक विकृत प्राण की ही निशानी होती है जिसे तीव्र संवेदनों की और अपने भड़के हुए अहंकार की तुष्टि की चाह होती है जो उसे शरीर को यंत्रणा प्रदान करके प्राप्त होती है। पंरतु गीता का तप तो बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का है। ब्रह्मचर्य के विषय में श्रीअरविन्द जो कहते हैं वह बहुत ही उद्बोधक है। वे कहते हैं, "अंतःस्थित शक्ति को बढ़ाने और उसे ऐसे उपयोगों में लाने की, जो उसके धारक को या मानवजाति को लाभान्वित करे, पहली और अत्यंत आवश्यक शर्त है ब्रह्मचर्य का अभ्यास । सारी मानवी शक्ति का एक भौतिक आधार होता है। युरोपीय भौतिकवाद द्वारा की गई भूल यह है कि वह भौतिक आधार को ही सर्वस्व और भ्रमवश मूल-स्रोत मान बैठता है। जीवन तथा शक्ति का स्रोत भौतिक नहीं, अपितु आध्यात्मिक है, किंतु जिस आधारशिला, नींव पर जीवन और शक्ति प्रतिष्ठित एवं क्रियाशील होती हैं, वह भौतिक है। प्राचीन हिंदू कारण और प्रतिष्ठा - सत्ता के ऊपरी और निचले छोरों - के बीच के भेद को स्पष्ट रूप से समझते थे। भू या स्थूल भौतिक तत्त्व प्रतिष्ठा है तथा ब्रह्म या आत्म-तत्त्व कारण है। भौतिक का अध्यात्म में उत्कर्षण ही ब्रह्मचर्य है, क्योंकि दोनों के सम्मिलन से वह शक्ति जो एक (ब्रह्म या आत्मा) से निसृत होकर दूसरे (भौतिक तत्त्व) को उत्पन्न करती है, वृद्धि को प्राप्त होती और स्वयं को चरितार्थ करती है।
यह ब्रह्मचर्य का तात्त्विक सिद्धांत है। इसका क्रियात्मक प्रयोग निर्भर होता है शक्ति के मानव आधार की भौतिक और मनोवैज्ञानिक रचना के ठीक-ठीक ज्ञान पर। मूलभूत भौतिक इकाई है रेतस्, जिसमें कि मनुष्य के अंतःस्थित तेजस्, अर्थात्, ऊष्मा और प्रकाश और विद्युत् शक्ति अंतर्निहित और छिपे पड़े हैं। सारी ऊर्जा रेतस् में निगूढ़ रूप से विद्यमान है। यह शक्ति या तो स्थूल भौतिक रूप में व्यय की जा सकती है या संरक्षित की जा सकती है। समस्त उत्तेजना, भोगेच्छा, कामना, इस शक्ति को स्थूल रूप में या एक उत्कृष्ट सूक्ष्मतर रूप में शरीर से बाहर फेंककर उसे नष्ट कर देती हैं। अनैतिक आचरण उसे स्थूल रूप में बाहर फेंक देता है; अनैतिक विचार सूक्ष्म रूप में। दोनों ही दशा में शक्ति नह होती है, और व्यभिचारिता जैसे शारीरिक होती है वैसे ही मानसिक और वाचिक भी होती है। इसके विपरीत, समस्त आत्म-संयम शक्ति को रेतस् में संरक्षित करता है और संरक्षण सदा ही अपने साथ संवर्द्धन लाता है। किंतु भौतिक शरीर की आवश्यकताएँ सीमित हैं और अतिरिक्त शक्ति से अवश्य ही उसके एक संचित भंडार का निर्माण होगा जिसे भौतिक के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में प्रयुक्त होना चाहिये। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार रेतस् जल है जो प्रकाश और ऊष्मा और विद्युत् से, एक शब्द में, तेजस् से परिपूर्ण है। रेतस् का अतिरेक सर्वप्रथम ऊष्मा या तपस् में परिवर्तित होता है, जो समस्त तंत्र को उद्दीप्त करता है, और इसी कारण आत्म-संयम और तपस्या के सभी रूपों को तपस् या तपस्या कहते हैं, क्योंकि वे ऊष्मा या उस उत्प्रेरक शक्ति को उत्पन्न करते हैं जो शक्तिशाली कर्म और सिद्धि का मूल-स्रोत है; द्वितीयतः, वह वास्तविक तेजस्, अर्थात् प्रकाश में, उस शक्ति में परिवर्तित होता है जो समस्त ज्ञान का उद्गम है; तृतीयतः, वह विद्युत् में रूपांतरित होता है जो सारे शक्तिशाली कर्म, चाहे बौद्धिक हो या शारीरिक, का आधार है। और फिर विद्युत् में निहित है ओजस् या प्राण-शक्ति, वह आदि-शक्ति जो आकाश से उत्पन्न होती है। रेतस् जल से तपस्, तेजस्, और विद्युत् में तथा विद्युत् से ओजस् में परिष्कृत होकर शरीर को शारीरिक बल, ऊर्जा और मेधा-शक्ति से भर देता है और अपने अंतिम स्वरूप ओजस् के रूप में ऊर्ध्वगामी होकर मस्तिष्क में पहुँचता है तथा उसे उस मूल ऊर्जा से अनुप्राणित कर देता है जो जड़-तत्त्व का सबसे परिष्कृत रूप है तथा आत्मतत्त्व के सबसे अधिक निकट है। वह ओजस् ही है जो आध्यात्मिक शक्ति या वीर्य को उत्पन्न करता है जिसके द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक प्रेम तथा श्रद्धा, आध्यात्मिक बल प्राप्त करता है। इसका निष्कर्ष यह है कि जितना ही हम ब्रह्मचर्य के द्वारा तपस्, तेजस्, विद्युत् और ओजस् के भंडार को अधिक बढ़ा सकेंगे, उतना ही अधिक हम स्वयं को शरीर, हृदय, मन और आत्मा के कार्यों के लिए पूर्ण-विशुद्ध शक्ति से भर देंगे।" (CWSA 1: 372-73)
प्रश्न : यहाँ 'पूजा' से क्या अभिप्राय है?
उत्तर : पूजा से तात्पर्य है कि देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी को उच्चासन पर प्रतिष्ठित करना, उनका सम्मान करना, उन्हें महत्त्व देना और उन्हें ही वास्तव में अनुकरणीय मान कर उनकी आज्ञापालन करना। बहुत बार व्यक्ति द्विज, गुरु आदि के सामने हाथ जोड़ कर, उन्हें प्रणाम आदि करके उनके प्रति आदर व्यक्त तो करता है परंतु अपने मन में वह उनके प्रति अवज्ञा का भाव रखता है, इस अर्थ में कि वह अपने ही बाहा जीवन की श्रेष्ठता का भाव रखता है और गुरुजन के पास जाकर भी अपनी संपत्ति, सुख-साधन, अपने प्रभावक्षेत्र आदि के अहंकार से भरा रहता है। परंतु जिस तपी का गीता यहाँ उल्लेख करती है वह ऐसा नहीं होता। वह तो देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी को वास्तव में ही श्रेष्ठ मानता है और उनके प्रति उसी भाव से अपनी क्रिया करता है। ये सारे गुण भी शारीरिक चेतना से ही सम्बद्ध हैं हालाँकि इन्हें करने में मनोविज्ञान भी साथ में रहता है। गीता जिन शारीरिक तपों का वर्णन करती है वे ही इतने असाध्य प्रतीत होते हैं कि इन्हें कर पाना तो एक बहुत लंबे अनुशासन और अभ्यास की माँग करता है।
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।। १५।।
१५. आघात न पहुँचाने वाली, सत्य, प्रिय और हितकर बोलने वाली वाणी को, तथा शास्त्रों के नियमित स्वाध्याय को वाणी के तप कहते हैं।
गीता शारीरिक तपस्या के बाद अब जिस वाणी की तपस्या का निरूपण कर रही है वह तो और भी अधिक सूक्ष्म है और जिस प्रकार की हमारी प्रकृति है, जिसमें अंध वृत्तियों, काम-क्रोधादि रिपुओं का हमारे ऊपर अधिकार रहता है, ऐसे में सच्चे रूप में सत्य, प्रिय और हितकर वाणी बोलना तो लगभग असंभव-सा प्रतीत होता है। और यह प्रिय और हितकर वाणी भी केवल कोई बाहरी रूप से प्रिय बोलना नहीं अपितु सच्चे अर्थों में ऐसा करना है। साथ ही, स्वाध्याय, अर्थात् अपने आप का अध्ययन किये बिना तो हम अपना संतुलन बनाए नहीं रख सकते। स्वाध्याय तो संतुलन का आधार है। वाणी की तपस्या या संयमन के विषय में श्रीमाताजी के शब्द बड़े ही प्रकाशक हैं। वे कहती हैं, "मानसिक संयम या तपस्या का प्रश्न मन में तुरंत ही उन लंबे घ्यानों की छवि ले आता है जो विचारों पर नियंत्रण और उसकी परिणति के रूप में आंतरिक नीरवता की ओर ले जाते हैं। योग-साधना का यह पक्ष इतना सुपरिचित है कि इसके बारे में विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। किंतु इसका एक और पक्ष भी है जिस पर प्रायः कम ध्यान दिया जाता है, वह है वाणी का संयम। बहुत ही विरले अपवादों को छोड़कर, साधारणतः गपबाजी या बेमतलब की बातचीत के विरुद्ध पूर्ण मौन को ही खड़ा किया जाता है। और फिर भी वाणी का नियंत्रण करना पूर्ण निरोध की अपेक्षा अधिक महान् और फलप्रद तपस्या है।
...हालाँकि, व्यक्ति को यह न समझना चाहिये कि बोले हुए शब्दों का मूल्य बातचीत के विषय पर निर्भर है। तुम आध्यात्मिक विषयों पर भी उसी तरह व्यर्थ में बकवाद कर सकते हो जैसे अन्य किसी भी विषय पर, और इस प्रकार की बकवाद सबसे अधिक भयंकर बकवादों में से एक हो सकती है। उदाहरण के लिये, नया साधक जो थोड़ा बहुत जानता है उसे औरों में बाँटने के लिये बहुत उत्सुक रहता है। परंतु जैसे-जैसे वह मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसे अधिकाधिक पता लगता है कि वह बहुत अधिक नहीं जानता और दूसरों को सिखाने का प्रयास करने से पहले उसे अपने ज्ञान के मूल्य के बारे में निश्चित होना चाहिये, जब तक कि अंत में वह बुद्धिमान् न हो जाए और यह अनुभव न करने लगे कि कुछ मिनटों तक उपयोगी बात करने के लिये घंटों की नीरव एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, जहाँ आंतरिक जीवन और आध्यात्मिक साधना की बात आती है, वाणी के उपयोग पर और भी अधिक कठोर अनुशासन रखना होगा और जब तक बिल्कुल ही आवश्यक ही न हो तब तक कुछ न कहा जाये।...
....अंत में निष्कर्ष स्वरूप, मैं यह कहूँगीः यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाणी सत्य को अभिव्यक्त करे और 'शब्द' की शक्ति प्राप्त करे तो कभी भी पहले से मत सोचो कि तुम क्या कहना चाहोगे, यह निश्चय न करो कि क्या कहना अच्छा या बुरा होगा, तुम जो कहने वाले हो उसके प्रभाव के बारे में हिसाब न लगाओ। अपने मन में नीरव रहो और 'सर्व-प्रज्ञा', 'सर्व-ज्ञान', 'सर्व-चेतना' के प्रति सतत् अभीप्सा के सच्चे भाव में स्थिर रहो। तब, यदि तुम्हारी अभीप्सा निष्कपट है, यदि यह खूब संपदा-संपन्न होने और सफल होने की महत्त्वाकांक्षा को छिपाने के लिये एक आवरण नहीं है, यदि वह शुद्ध, सहज और सर्वांगीण है, तो तुम सरलता के साथ बोल सकोगे, वही शब्द बोलोगे जो बोले जाने चाहिये, न अधिक, न कम, और उनमें सृजनशील शक्ति होगी।" (CWM 12, 57-64)
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।। १६ ।।
१६. मन की शांत-चित्तता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम, विचारों की शुद्धता, इन्हें मानस तप कहा जाता है।
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः ।
अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ।। १७।।
१७. योगयुक्त लोगों द्वारा, फल की कामना से रहित हो परम श्रद्धा के साथ इस त्रिविध तप का अनुष्ठान करना सात्त्विक कहा जाता है।
इसमें वे सभी चीजें समाविष्ट हो जाती हैं जो राजसिक एवं अहंकारमय प्रकृति को शांत या अनुशासित करती हैं और वे सब भी जो इसके स्थान पर शुभ और पुण्य के सुखद और शांत तत्त्व की प्रतिष्ठा करती हैं। यह सात्विक धर्म का तप है जिसे प्राचीन भारतीय संस्कृति की व्यवस्था में इतना अधिक महत्त्व प्रदान किया गया था। इसकी इससे महत्तर परिणति होगी बुद्धि और संकल्प की एक उच्च पवित्रता, आत्मा की समता, गंभीर शांति और स्थिरता, व्यापक सहानुभूति तथा एकत्व की तैयारी, अंतःपुरुष के दिव्य हर्ष की मन, प्राण और शरीर के अंदर एक झलक या आभास। वहाँ उस उच्च शिखर पर नैतिक आदर्श तो पहले ही आध्यात्मिक प्रकार और स्वरूप में परिणत होने लगता है। और इस परिणति को भी अपने-आप को अतिक्रम कराया जा सकता है, इसे भी एक उच्चतर और मुक्ततर ज्योति में उन्नीत किया जा सकता है तथा यह भी परा प्रकृति की शांत-स्थिर देवतुल्य शक्ति में परिणत हो सकती है। और तब जो कुछ शेष रहेगा वह होगा आत्मा का निर्मल या शुद्ध तपस्, सत्ता के सभी अंगों में एक उच्चतम संकल्प एवं ज्योतिर्मय शक्ति, जो विशाल और ठोस शांति तथा गंभीर एवं विशुद्ध आनंद में कार्य करेगी। तब फिर तप की और आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई तपस्या नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ सहज-स्वाभाविक रूप से दिव्य होगा, सब कुछ वह तपस् ही होगा। वहाँ नीचे की शक्ति का कोई पृथक् परिश्रम नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति की शक्ति पुरुषोत्तम के परात्पर संकल्प में अपना सच्चा उद्गम और आधार प्राप्त कर चुकी होगी। तब, इस उच्च स्रोत से प्रवर्तित होने के कारण, इस शक्ति की क्रियाएँ निम्नतर स्तरों पर भी एक सहजात पूर्ण संकल्प से तथा एक अंतर्निहित पूर्ण मार्गनिर्देशक के द्वारा स्वाभाविक एवं स्वतः-स्फूर्त रूप में निःसृत होगी। किन्हीं भी वर्तमान प्रचलित धर्मों में से किसी का भी बंधन नहीं रहेगा: क्योंकि वहाँ एक मुक्त कर्म होगा जो राजसिक और तामसिक प्रकृति से बहुत ऊपर तो होगा ही पर साथ ही कर्म के सात्त्विक नियम की अति-सतर्क और संकीर्ण सीमाओं से भी बहुत परे होगा।
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्पेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ।। १८ ।।
१८. दिखावे के लिए और मनुष्यों से सत्कार, मान और पूजा प्राप्त करने के हिये जो तप किया जाता है, उसे यहाँ राजसिक कहा जाता है; यह अस्थिर और अनित्य होता है।
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
रस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ।। १९।।
१९. जो तप मूढ़ दुराग्रह, आत्म-उत्पीड़न के सहित या दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसे तामसिक कहा जाता है।
तपस्या की भाँति समस्त दान भी अज्ञ तामसिक, बाह्याडंबरपूर्ण राजसिक या निःस्वार्थ और ज्ञानदीप्त सात्त्विक प्रकृति का होता है।
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।। २० ।।
२०. जब दान दान के ही भाव से दिया जाए, उसको दिया जाए जिससे कोई प्रतिफल की अपेक्षा न की जाती हो, और उचित स्थान पर दिया जाए, उचित समय पर दिया जाए और उचित पात्र को दिया जाए, उस दान को सात्त्विक कहा गया है।
सात्त्विक प्रकार के दान की पराकाष्ठा कर्म के अंदर दूसरों के प्रति, जगत् तथा परमेश्वर के प्रति एक व्यापक आत्मदान एवं आत्म-समर्पण के तत्त्व को क्रमशः अधिकाधिक ले आएगी जो कि गीता द्वारा प्रतिपादित कर्मों के यज्ञ का उच्च उत्सर्ग ही है। दिव्य प्रकृति में ऊर्ध्वतम स्थिति आत्म-दान की महत्तम परिपूर्णता होगी जो जीवन के विशालतम अर्थ पर आधारित होगी। यह समस्त बहुविध विश्व भगवान् द्वारा इन सब भूतों को अपना स्वयं का और अपनी शक्ति का दान करने के कारण और इन सब भूतों में अपनी सत्ता और आत्मा को मुक्तहस्त प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है और सतत् स्थितिशील रहता है; वेद कहता है कि विश्व-सत्ता पुरुष का यज्ञ है। सिद्ध जीव का भी समस्त कर्म होगा - अपना तथा अपनी शक्तियों का इसी प्रकार सतत् रूप से दिव्य दान करना, भगवान् के अंदर तथा उनके प्रभाव और प्रेरणा के द्वारा उसने जो ज्ञान, ज्योति, बल, प्रेम, हर्ष, साहाय्यप्रद शक्ति उपलब्ध की है उसे अपने चारों ओर सबके ऊपर, उनकी ग्रहण-सामर्थ्य के अनुसार उँड़ेल देना, अथवा इस समस्त जगत् तथा इसके प्राणियों पर प्रवाहित कर देना। हमारी सत्ता के स्वामी के प्रति जीव के समग्र आत्मदान का संपूर्ण परिणाम यही होगा।
यह समग्र आत्मदान निखैगुण्य होता है। भगवान् से हमें जो भी ज्ञान, ज्योति, बल, प्रेम, हर्ष, साहाय्यप्रद शक्ति प्राप्त होती है उसे अपने चारों ओर सबके ऊपर, उनकी ग्रहण-सामर्थ्य के अनुसार उँडेल देना होगा।
देश, काल और पात्र का विचार करके किये जाने वाला दान तो सात्त्विक होता है परन्तु सहज रूप से भगवद् प्रेरणा से सब पर ही उँड़ेल देना नित्रैगुण्य होता है, जैसे परमात्मा अपना प्रेम सभी प्राणियों पर समान ही रूप से उँड़ेलते हैं चाहे वह नास्तिक हो अथवा आस्तिक, पापी हो अथवा पुण्यात्मा।
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ।। २१ ।।
२१. जो दान अनिच्छापूर्वक किसी प्रकार के बदले की आशा से अथवा किसी प्रतिफल की इच्छा से या किसी फल तथा पुरस्कार की दृष्टि से दिया जाता है वह दान राजसिक कहा जाता है।
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ।। २२।।
२२. जो दान अनुपयुक्त देश और काल में तथा अयोग्य पात्र को तिरस्कार और अवहेलनापूर्वक दिया जाता है वह तामसी कहा जाता है।
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिताः पुरा ।। २३ ।।
२३. ॐ-तत्-सत्, इसे ब्रह्म की त्रिविध परिभाषा या व्याख्या कहते हैं जिसके द्वारा पूर्व काल में ब्राह्मण और वेद और यज्ञ सृष्ट हुए हैं।
गीता इस अध्याय का उपसंहार एक ऐसे कथन से करती है जो प्रथम दृष्टि में दुर्बोध प्रतीत होता है। वह कहती है कि ॐ, तत्, सत्, यह सूत्र उन ब्रह्म की त्रिविध परिभाषा है जिनके द्वारा पुराकाल में ब्राह्मणों, बेदों और यहाँ की सृष्टि हुई थी और इसी सूत्र में उनका समस्त गर्भित अर्थ निहित है। 'तत् निरपेक्ष सत्ता का द्योतक है। 'सत्' परम् और विश्वमय सत्ता के मूलतत्त्व का द्योतक है। 'ओम्' त्रिविध ब्रह्म का, बहिर्मुख, अन्तर्मुख या सूक्ष्म तथा अतिचेतन कारण-पुरुष का प्रतीक है। अ, उ, म - यह प्रत्येक अक्षर इन तीन में से एक-एक को आरोहण-क्रम में द्योतित करता है और अपने समूचे रूप में यह अक्षर उस तुरीय अवस्था का बोधक है जो निरपेक्ष सत्ता की ओर उठ जाती है।
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ।। २४।।
२४. इसलिये शाखविधान के अनुसार प्रतिपादित यज्ञ, दान, तप की क्रियाओं को ब्रह्मवादियों के द्वारा सदा ही ॐ के पूर्व-उच्चारण द्वारा आरंभ किया जाता है।
तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपः क्रियाः ।
दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ।। २५।।
२५. मोक्ष की इच्छा रखनेवाले व्यक्तियों के द्वारा फल की कामना के बिना और तत् के उच्चारण के साथ ही यज्ञ, तप और दान की विविध क्रियाओं का अनुष्ठान किया जाता है।
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ।। २६॥
२६ . हे पार्थ। यथार्थता या सत्तत्व के और श्रेष्ठता के अर्थ में सत् शब्द का प्रयोग होता है और श्रेष्ठ कर्म के अर्थ में भी सत् शब्द प्रयुक्त होता है।
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।। २७।।
२७. यज्ञ, तप तथा दान में दृढ़प्रतिष्ठा भी सत् कही जाती है और तत् के लिये किये जाने वाले समस्त कर्म भी सत् ही कहे जाते हैं।
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ।। २८ ।।
२८. हे पार्थ! हवन, दान, तप या अन्य कोई कर्म, जो कुछ भी बिना श्रद्धा के किया जाता है वह असत् कहा जाता है; वह इस लोक में और परलोक में व्यर्थ अथवा निष्फल है।
और क्योंकि श्रद्धा हमारी सत्ता का केंद्रीय तत्त्व है, इनमें से कोई चीज यदि बिना श्रद्धा के की जाए तो वह एक मिथ्यात्व होती है, इहलोक में या परतर लोकों में उसका कोई सच्चा अर्थ या सच्चा सार नहीं होता, इह-जीवन में या मर्त्य जीवन के पश्चात् हमारी चिन्मय आत्मा के महत्तर लोकों में टिके रहने या सृजन करने के लिए उसमें कोई सत्य या शक्ति नहीं होती। अंतरात्मा विश्वास ही नहीं करने तथा अपनी दृष्टि और ज्ञान के अनुसार कर्म करने तथा अपने को गढ़ने के लिए अंतरात्मा का एकाग्र संकल्प ही अपनी शक्ति के द्वारा हमारे विकास की या अभिव्यक्ति की संभावनाओं की मर्यादा निर्धारित करता है, और हमारी संपूर्ण बाह्यान्तर सत्ता, प्रकृति और कर्म के सहित उस सबकी ओर - जो कुछ उच्चतम, दिव्यतम, सत्यतम और शाश्वत है - मुड़ी हुई यह श्रद्धा एवं संकल्प ही है जो हमें परम सिद्धि की प्राप्ति में समर्थ बना देगा।
श्रद्धा ही प्रधान तत्त्व है जो हमारी गहराइयों से आती है। आखिर श्रद्धा की आवश्यकता क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी मानसिक, प्राणिक और भौतिक सत्ता सीमित है अतः यह न तो परात्पर के संकल्प को समझ सकती है और न उसे अभिव्यक्त कर सकती है। श्रद्धा हमें उस कार्य में नियोजित करती है जिसे समझने के लिए हमारी बुद्धि अक्षम होती है। परंतु सभी विपरीत और विषम प्रतीतियों के बावजूद भी श्रद्धा हमें उस संकल्प के प्रति लगाये रखती है। यदि ऐसा न होता तो जिस प्रकार की भौतिक और मानसिक चेतना की संरचना में हम फंसे रहते हैं उसमें से कभी निकल ही नहीं सकते थे। यह तो एक प्रकार से उच्चतर स्तरों से निम्नतर स्तरों पर डाली गई वह डोरी है जिसकी सहायता से व्यक्ति ऊपर चढ़ सकता है। व्यक्ति से यह वह कार्य संसिद्ध करा लेती है जो कि उसकी सोच-समझ आदि के सर्वथा विपरीत भी हो सकता है।
जैसे-जैसे हमारी चेतना का विकास होता है वैसे-वैसे फिर यह श्रद्धा ज्ञान का रूप ले लेती है। परन्तु कितना भी विकास क्यों न हो जाये फिर भी हम देखेंगे कि किन्हीं क्षणों पर श्रद्धा की आवश्यकता बनी ही रहती है क्योंकि मानव बुद्धि चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो जाए फिर भी पूरी तरह से दिव्य जननी की क्रिया को भला कितना समझ सकती है। साथ ही, स्वयं श्रद्धा का रूप भी बदलता रहता है और यह उत्तरोत्तर वर्धित होती रहती है। तब स्वयं अपने जीवन में भी हम ऐसे कार्यों को सहज रूप से करने लगते हैं, भले सचेतन रूप से या फिर अभ्यासवरा, जो किन्हीं भी बाहरी मानदंडों से या तो बिल्कुल असंभव प्रतीत होते हैं ग मानसिक दृष्टिकोण से बिल्कुल असंगत प्रतीत होते हैं। श्रीअरविन्द ने अपनी कृतियों में श्रद्धा के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है।
प्रश्न : ॐ-तत्-सत् में जो तत् है उसे निरपेक्ष सत्ता बताया गया है। निरपेक्ष सत्ता से क्या तात्पर्य है?
उत्तरः श्रीमाँ के अनुसार ॐ भगवान् का हस्ताक्षर है। उनका नाम है। तत् अर्थात् 'वह' और सत् का तात्पर्य है संभूति। ब्रह्म की अभिव्यक्ति बहुत जटिल है। सम्पूर्ण ब्रह्मांड ॐ की मूल ध्वनि से ही उत्पन्न हुआ है। इसको मनुष्य का मन नहीं समझ सकता। बीज मंत्रों में "ॐ ह्रीं क्लीं" आदि विभिन्न प्रकार के नाद का क्या तात्पर्य है इसको हमारा मन कभी समझ नहीं सकता। नाद मन की अपेक्षा अधिक गहन है और विशालतर अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। इसीलिये भारतीय सभ्यता में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। अतः माना जाता है कि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वे सृष्टि क्रिया को सशक्त बना कर उसे अधिक समृद्ध बनाते हैं। परंतु यह रहस्य अब लुप्त हो गया है।
यदि हम उच्चतर चेतना से जुड़े हों तो सब कुछ केवल संकल्प मात्र से ही साधित कर सकते हैं। तब हमारे मन में जो विचार है वह भी बहुत प्रभावशाली बन जाता है। तब कहने मात्र से वांछित चीज का निर्माण किया जा सकता है। यह संकल्प सब व्यवस्था करने में सक्षम है। गुह्यवेत्ताओं का मानना है कि संसार में जितने भी महत् कार्य तथा महान् क्रांतियाँ हुई हैं वे सब भी ऋषियों के संकल्प का ही परिणाम हैं जो भौतिक रूप से अपने तरीके से अभिव्यक्त होती हैं। श्रीमाताजी की क्रिया भी जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार संकल्प मात्र से वे अपनी क्रिया संसिद्ध करती थीं। अन्यथा वैश्विक स्तर पर तो क्रिया करने का और कोई दूसरा साधन ही नहीं है।
इस प्रकार सत्रहवाँ अध्याय 'श्रद्धात्रयविभागयोग' समाप्त होता है।
अठारहवाँ अध्याय
I. त्रिगुण, मन और कर्म
त्रिगुण के विषय में, तथा उच्चतम सात्त्विक साधना की अपने आप को अतिक्रम करने वाली पराकाष्ठा के द्वारा गुणों से परे त्रिगुणातीता को भी आने के मूलभूत विचार के प्रकाश में गीता ने कर्म के विश्लेषण को अपने जक संपूर्ण नहीं किया है। श्रद्धा, अर्थात् जो सत्य हमने देख लिया है उस पा विश्वास करने, वही बन जाने, उसे जानने, उसे जीने तथा कार्य-रूप में परिणत करने का संकल्प ही है जो किसी स्वयं-विकसनशील कर्म के पीछे, और सबसे बढ़कर, कर्मों के द्वारा जीव के अपनी पूर्ण आध्यात्मिक महत्ता या स्थिति में विकसित होने के पीछे स्थित प्रधान तत्त्व, अपरिहार्य शक्ति है। परन्तु इसके साथ ही मानसिक शक्तियाँ, उपकरण या साधन एवं अवस्थाएं भी हैं जो कर्म की गति, दिशा तथा स्वरूप का गठन करने में सहायक होती हैं और इसलिए इस मनोवैज्ञानिक या आंतरिक साधना की पूर्ण समझ प्रात करने में महत्त्व रखती हैं। इससे पहले कि गीता अपने उस महान् चरम सिद्धान्त की ओर, जो कुछ शिक्षा वह देती है उसकी परिणति की ओर, उस उच्चतम रहस्य की ओर जो कि सभी धर्मों के आध्यात्मिक अतिक्रमण का रहस्य है, एक दिव्य परात्परता की ओर अग्रसर हो, वह इन तत्त्वों (मानसिक शक्तियों आदि) का संक्षिप्त मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आरंभ करती है।
विषय के इस अंश की चर्चा अर्जुन के एक अंतिम प्रश्न के द्वारा आरम्भ की गयी है जिसमें वह संन्यास और त्याग के तत्त्व तथा इनके भेद के विषय में पूछता है।
इस अध्याय के प्रथम उनचालीस श्लोकों में गीता जिस तत्त्व का निरूपण करने जा रही है श्रीअरविन्द ने उसका यहाँ संकेत कर दिया है। इस अंश में श्रीअरविन्द ने जीवन की जिस सबसे महत्त्वपूर्ण और मूलभूत बात की ओर संकेत किया है वह है श्रद्धा, 'अर्थात् जो सत्य हमने देख लिया है उस पर विश्वास करने, वही बन जाने, उसे जानने, उसे जीने तथा कार्यरूप में परिणत करने का संकल्प ही है जो किसी स्वयं-विकसनशेत कर्म के पीछे, और सबसे बढ़कर, कर्मों के द्वारा जीव के अपनी पूर्ण आध्यात्मिक महत्ता या स्थिति में विकसित होने के पीछे स्थित प्रधान तत्त्व, अपरिहार्य शक्ति है।' यह केवल आध्यात्मिक साधना का ही मूलभूत सत्य नहीं है अपित हमारे सारे जीवन का भी सार है। कोई भी मनुष्य बिना श्रद्धा के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। श्रद्धा वह सत्य है जिसे यिक्ति का मन भले ही न समझता हो परन्तु जिसे व्यक्ति ने भीतर से देख लिया होता है। श्रद्धा व्यक्ति को सत्य का आस्वादन प्रदान कर देती है।
प्रश्न : क्या सत्य को देख लेने का अर्थ ही उसे अनुभव करना है?
उत्तर : उदाहरण के लिए, जब हम किसी चित्र को देख लेते हैं तो दृष्टि के द्वारा उसके विषय में सुनिश्चित हो जाते हैं। उसी प्रकार जब श्रद्धा के माध्यम से हम सत्य को देख लेते हैं तब इस विषय में पूर्णतः आश्वस्त हो जाते हैं कि सत्य क्या है भले ही मानसिक रूप से हम उसे न समझते हों। उदाहरण के लिए, आध्यात्मिक जीवन में अधिकांशतः ही ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अपने लिए नियत गुरु के पास जाता है तब भले ही उसे उसके अनुभवों, सिद्धियों आदि के बारे में कुछ भी पता न हो परंतु भीतर से श्रद्धा स्पष्ट रूप से यह जान जाती है कि वही व्यक्ति उसे उसके गंतव्य तक ले जा सकता है। इसी श्रद्धा के आधार पर व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन, भाव, कर्म, सर्वस्व अनन्य रूप से गुरु रूप में स्वीकार कर उसे समर्पित कर देता है और उसी श्रद्धा के आधार पर वास्तव में अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है। भले ही स्वयं गुरु को अमुक दर्शन या सिद्धि प्राप्त हो या न हो, परंतु अपनी श्रद्धा के प्रभाव से व्यक्ति को उसके माध्यम से जो कुछ भी आवश्यक है वह निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा एक बड़ा ही अद्भुत विधान है। यदि भीतर श्रद्धा न हो और केवल बाहरी व्यक्तित्व से, सिद्धियों आदि से ही प्रभावित होकर व्यक्ति किसी गुरु के पास जाता है तो उसे उससे कोई भी सच्चा लाभ नहीं हो सकता क्योंकि स्वीकार तो व्यक्ति वही करता है जो भीतर से उसकी श्रद्धा होती है अन्यथा तो जैसे बाजार में व्यक्ति देखता-परखता तो हजारों चीजें हैं परंतु खरीदता वही है जो उसी खरीदना होता है और कभी-कभी तो कुछ भी नहीं खरीदता, उसी प्रकार श्रद्धा के अभाव में व्यक्ति जीवन भर सौदेबाजी भले ही कर सकता है परंतु वास्तव में उसे कोई सच्ची उपलब्धि नहीं होती।
इसीलिये तो रामायण में बालकाण्ड में तुलसीदास जी कहते हैं -
भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ।।
अर्थात् श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्रीपार्वतीजी और श्रीशंकरजी की मैं वन्दना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अन्तःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते।
यदि हम श्रद्धा के इस तत्त्व को केवल गीता के ही परिप्रेक्ष्य में न देखकर व्यापक अर्थ में भली प्रकार समझ सकें तो हम यह स्पष्टतः देख पाएँगे कि किस प्रकार हमारा सारा जीवन श्रद्धा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, अपितु उसी का परिणाम है। हमारा भावी जीवन भी हमारी वर्तमान श्रद्धा का ही परिणाम होगा। जिसे हम सामान्य तौर पर आध्यात्मिक जीवन कहते हैं केवल उसी में नहीं अपितु सामान्य जीवन में भी श्रद्धा अपरिहार्य तत्त्व है। जब व्यक्ति के मन में भीतरी श्रद्धा की प्रतिछाया के रूप में यह प्रबल विचार आता है कि उसे अमुक पेशे में जाना है, उद्योग, कृषि, खेल, राजनीति, अभिनय या फिर अन्य किसी क्षेत्र में जाना है तब वह उस विचार की दिशा में अपनी सारी ऊर्जा, अपना संकल्प और उपलब्ध संसाधन लगाता है। अपने पेशे के इस चयन का हम भले ही कोई बाहरी कारण बता सकते हैं, परंतु वास्तव में तो यह चयन भीतर की श्रद्धा के आधार पर होता है भले वह श्रद्धा तामसिक हो, या राजसिक हो या फिर सात्त्विक हो। और व्यक्ति जितना ही अधिक एकाग्र रूप से अपने चयनित क्षेत्र की दिशा में अपनी ऊर्जा लगाता है उतना ही अधिक वह उसमें सफल होता है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा जितनी ही प्रखर होती है उतना ही प्रखर, दृढ़ और एकनिष्ठ उसका संकल्प होता है और उसी के अनुपात में उसकी उपलब्धि होती है। वहीं यदि किसी में श्रद्धा सुस्पष्ट न हो, उसका संकल्प भी दृढ़ न होकर विचलित होता रहता हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अधिक कुछ संसिद्ध नहीं कर पाता। अतः साधारण जीवन में भी श्रद्धा के बिना व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। श्रद्धा तो परमात्मा का रूप ही है इसलिए यदि वह अटल रूप से आ जाती है तो निश्चित ही चरितार्थ होती है।
कोलम्बस के ही उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एकमात्र श्रद्धा के आधार पर उसने अपना समुद्री अभियान शुरू किया था। जिस समय उसने व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने का निश्चय किया उस समय किसी को भी सही-सही भौगोलिक ज्ञान न होने के कारण कोई भी उसके साथ यात्रा पर जाने के लिए तैयार न था। अन्य कोई जब उसके साथ जाने के लिए तैयार न था तब उसे सजा काट रहे कैदियों को मजबूरन अपने साथ यात्रा पर ले जाना पड़ा। यहाँ तक कि वे भी यात्रा की बजाय कैद में ही रहना अधिक पसंद कर रहे थे। किया ही, सभी को यह भय था कि एक सीमा के बाद समुद्र का अंत आते ही सभी धरती से बाहर गिर जाएँगे। यात्रा के दौरान भी जब बहुत समय तक दूर-दूर तक समुद्र ही दिखाई देता था तब सभी समय-समय पर हताश होकर बहुत विचलित हो जाते थे और भयभीत हो जाते थे। यही नहीं, जहाजी दल ने समय-समय पर कोलंबस को मार डालने की भी योजना बनाई ताकि उससे पीछा छुड़ाकर पुनः लौट सकें भले पुनः लौटकर उन्हें कैद में ही क्यों न रहना पड़े। ऐसे में केवल भीतर से श्रद्धा ही थी जिसने कोलम्बस को डटे रहने की शक्ति दी। अंततः जब एक दिन उन्होंने आसमान में पक्षी देखे, पानी में फल लगी पेड़ की बहती हुई शाखा देखी तब उन्हें राहत की साँस मिली कि जमीन पास ही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्रद्धा कैसी प्रबल शक्ति है जिसके सहारे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है भले ही उसकी बाहरी प्रकृति कंपित और विचलित ही क्यों न हो रही हो। आध्यात्मिक जीवन में तो श्रद्धा के बिना कुछ भी संसिद्ध हो ही नहीं सकता।
अर्जुन उवाच
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ।। १।।
१. अर्जुन ने कहाः हे महाबाहो ! मैं संन्यास और त्याग के तत्त्व को जानने की इच्छा रखता हूँ, और हे हृषीकेश। उनके भेद' को भी जानना चाहता हूँ, हे केशिनिषूदन (केशि नामक दैत्य का विनाश करनेवाले श्रीकृष्णा)।
श्रीभगवान् उवाच
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ।। २॥
२. श्रीभगवान् ने कहाः ऋषियों ने कामना द्वारा प्रेरित किये गये कमाँ के परित्याग को संन्यास माना है; और समस्त कमाँ के फल के परित्याग को ज्ञानियों द्वारा त्याग कहा जाता है।
इस अर्थ में संन्यास नहीं त्याग ही श्रेयस्कर मार्ग है। जिस चीज का त्याग करने की आवश्यकता है वह कामनात्मक कर्म नहीं हैं अपितु उस कामना को हमसे दूर कर देने की आवश्यकता है जो कर्म को वैसा कामनात्मक स्वरूप प्रदान कर देती है। कर्मों के प्रभु के विधान के अंदर कर्म का फल प्राप्त हो सकता है, किन्तु कर्म करने के पुरस्कार या उसकी शर्त के रूप में फल की कोई अहंपूर्ण माँग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि फल बिल्कुल भी न मिले और फिर भी हमें कर्म को 'कर्तव्यं कर्म' (एक करने योग्य कर्म) के रूप में करना ही चाहिए, वह चीज जिसकी हमारे अंतःस्थ प्रभु हमसे माँग करते हैं। सफलता और विफलता उन्हीं के हाथों में है और उन्हें वे अपने सर्वज्ञ संकल्प तथा अबोधग्राह्य प्रयोजन के अनुसार निर्धारित करेंगे। कर्म का, वस्तुतः समस्त कर्म का, अंत में त्याग करना होगा, (परंतु) ऐसा भौतिक रूप से, कर्म का परिहार करके, निश्चल-निष्क्रिय रह कर नहीं, अपितु आध्यात्मिक रूप से, हमारी सत्ता के उन स्वामी के प्रति कर्मों का त्याग करना होगा केवल जिनकी ही शक्ति से कोई भी कर्म संसिद्ध किया जा सकता है। अपने आप को कर्त्ता के रूप में मानने के मिथ्या विचार का त्याग करना होगा;
__________________________________
*गीता का इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण भेद को प्रायः ही गुंजारित करना, बारंबार इस पर बल देना उत्तरकालीन भारतीय मन के परवर्ती इतिहास द्वारा यथेष्ट रूप से औचित्यपूर्ण सिद्ध कर दिया गया है क्योंकि यहाँ हम भारतीय मन को इन दो अत्यंत भिन्न विषयों में निरंतर ही विभ्रम अथवा अस्तव्यस्तता की स्थिति में देखते हैं और गीता द्वारा कर्म के विषय में दी गई इस भूम अथवा अस्तव्यस्तताक की अधिक-से-अधिक संन्यास के परम देखते की एक प्रारम्भिक अवस्था के रूप में गौण महत्त्व प्रदान किये जाने की हैं। सच पूछो तो, जब प्रबल प्रवृत्ति लोग त्याग की बात करते हैं तब वे इस शब्द का जो अर्थ समझते हैं या कम-से-कम इसके जिस अर्थ पर वे बल देते हैं, वह सदा जगत् का बाह्य त्याग ही होता है, जब कि कैम इसके जिस से विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है कि वास्तविकता नगरतर में कर्म करने और जीवन यापन करने को अपने आधार है मठ-मंदिर, गुहा-कंदरा या गिरि-श्रृंग की ओर पलायन को। यथार्थ त्याग है कामना को त्याग कर कर्म करना और यथार्थ संन्यास भी यही है।
क्योंकि वास्तव में यह विश्व-शक्ति ही है जो हमारे व्यक्तित्व तथा हमारे अहं के द्वारा कार्य करती है। गीता की शिक्षा में अपने सब कमर्मों को आध्यात्मिक रूप से प्रभु तथा उनकी शक्ति को सौंप देना ही सच्चा संन्यास है।
यहाँ मुख्य रूप से दो बातें समझाई गई हैं। एक तो यह कि कामनामय कर्मों का परित्याग कर देना चाहिये। किन्तु तब तो कर्म मात्र का हो त्याग करना होगा क्योंकि समस्त कर्मों की वर्तमान प्रेरक शक्ति तो कामना ही है। परंतु इसके उपाय के रूप में बताया गया है कि कर्मों का त्याग नहीं अपितु कर्मों को जो चीज दूषित करती है उसी का त्याग करना है। अपने आप में कोई भी कर्म खराब या अच्छा नहीं होता। उसके पीछे का भाव ही है जो उसे वैसा स्वरूप प्रदान कर देता है। परंतु यदि हम देखें तो वास्तव में न तो कर्मों का त्याग संभव है और न ही कामना का। यही दुविधा अर्जुन के सामने थी कि सामान्यतः तो हम कामों का चयन उनसे मिलने वाले फल के अनुसार या फिर किसी अप्रिय बीज से बचने के लिए करते हैं, परंतु यदि कर्मों के इस आधार को ही हटा दिया जाए तब फिर व्यक्ति कर्म का चयन किस आधार पर करेगा। इसी के समाधान के रूप में पहले ही गीता कह चुकी है कि कर्मों को यज्ञ रूप से और भगवान् की प्रसन्नता के निमित्त करने पर उनमें जो कामना का दोष है वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है और तब वे कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं। जब हम इस भाव से कार्य करते हैं कि श्रीमाताजी को, या फिर हमारे इष्ट को कौनसा कार्य पसंद होगा और कौनसा नहीं, तो इतने भर से भी कुछ निषिद्ध कर्म तो स्वतः ही बंद हो जाएँगे जिन्हें हम अभ्यासवश या फिर अचेतनतापूर्वक किये जा रहे थे। और ज्यों-ज्यों हम अधिकाधिक सचेतन होते जाएँगे त्यों-ही-त्यों हमें अधिक स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि कौनसे कर्म निषिद्ध हैं और कौनसे कर्म करने योग्य हैं। इस प्रकार यह भाव भी धीरे-धीरे हमारे कर्मों के संपूर्ण स्वरूप को ही बदल देता है। इस विषय में तो हम पहले भी विशद चर्चा कर चुके हैं।
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ।। ३।।
३. कुछ मनीषी लोग कहते हैं कि "समस्त कर्मों का इस प्रकार परित्याग कर देना चाहिये जैसे किसी दोष का"; और दूसरे ऐसा कहते हैं कि "यज्ञ, दान और तपरूप कमाँ का परित्याग नहीं करना चाहिये।"
फिर भी यह प्रश्न उठता है कि कौन-कौन से कर्म किये जाने चाहिये? जो लोग संपूर्ण बाह्य भौतिक त्याग का पक्ष लेते हैं वे भी इस गहन विषय में एकमत नहीं हैं। कुछ लोग यह कहेंगे कि सभी कर्मों को हमारे जीवन से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, मानो ऐसा करना संभव भी हो। परन्तु जब तक हम इस देह में हैं तथा जीवित हैं तब तक ऐसा संभव नहीं है; न ही मुक्ति इस बात में हो सकती है कि हम अपनी सक्रिय सत्ता को समाधि के द्वारा मिट्टी के ढेले और पत्थर के टुकड़े की-सी निर्जीव निश्चलता में परिणत कर दें।...तो फिर किये जाने वाले कर्म कौन से हैं? एक नैष्ठिक संन्यासवादी उत्तर यह होगा, जो कि गीता ने उल्लेख नहीं किया है - क्योंकि संभवतः यह उत्तर उस समय सर्वथा प्रचलित नहीं था – कि ऐच्छिक कर्मों के रूप में केवल भिक्षाटन, भोजन और ध्यान को ही स्वीकार करना होगा और वैसे इनके अतिरिक्त केवल आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को करना होगा। परंतु प्रत्यक्षतः ही इसका एक अधिक उदार और व्यापक समाधान था यज्ञ, दान और तप रूपी अत्यंत सात्त्विक क्रियाओं को जारी रखना। और गीता कहती है कि इन्हें अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि ये मनीषी को शुद्ध करते हैं।
कुछ मनीषी सारे ही कर्मों के परित्याग का प्रतिपादन करते हैं परंतु वास्तव में यह लागू करना संभव नहीं है क्योंकि कर्म केवल भौतिक हो नहीं अपितु प्राणिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। इसलिए कर्मों के परित्याग में केवल भौतिक कर्मों का परित्याग करने का प्रयास करना एक मूर्खतापूर्ण और असंगत बात है। कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। तब फिर कर्म किस प्रकार किये जाने चाहिये? इसके लिए कुछ मनीषी कर्मों को यज्ञ, तप और दान के रूप में करने का प्रतिपादन करते हैं। इस विषय में पहले ही हम विशद चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार यज्ञ, तप और दान शब्दों से जो हम केवल स्थूल भौतिक क्रियाओं से अर्थ लगाते हैं वही नहीं है, अपितु ये हमारी सत्ता और अस्तित्व मात्र के, सारी सृष्टि के मूलभूत तत्त्व हैं जिनके बिना यह सृष्टि ही नहीं हो सकती। जब हम इस व्यापक अर्थ में यज्ञ, तप और दान को समझते हैं तभी हमें यह अनुभव होता है कि इन पदों से गीता का जो अभिप्राय है वह वास्तव में कोई देश-काल मर्यादित विषय नहीं है जो कि किसी समय विशेष पर प्रासंगिक रहा हो परंतु अब जिसकी कोई प्रासंगिकता न रही हो। गीता के यज्ञ, तप और दान तो सभी समयों में, सभी स्थानों पर और सभी पर समान ही रूप से लागू होते हैं।
निश्वयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ।।४।।
४. हे भरतश्रेष्ठ! त्याग के विषय में मेरे मतों अथवा निर्णयों को सुन। हे पुरुषव्याघ्र (नरों में व्याघ्र के समान)! त्याग को त्रिविध बताया गया है।
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।। ५।।
५. यज्ञ, दान और तपरूप कमाँ का परित्याग नहीं करना चाहिये। यज्ञ, दान और तप मनीषियों को पवित्र करनेवाले हैं; इसलिए, उनका अवश्यमेव ही अनुष्ठान करना चाहिए।
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ।। ६।।
६. किंतु ये कर्म भी आसक्ति और फल की कामना का परित्याग करके किये जाने चाहिये। हे पार्थ। यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है।
अतः गीता इस पर बल देती है कि व्यक्ति को सदा ही यज्ञ, तप और दान का अनुष्ठान करते रहना चाहिये और वह भी आसक्ति रहित होकर भगवान् के प्रीत्यर्थ। आध्यात्मिक जीवन में तो ये क्रियाएँ अपरिहार्य हैं इसलिए कभी भी साधक को यज्ञ, तप और दान नहीं छोड़ने चाहिये। केवल इन्हीं के अनुष्ठान से साधक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है।
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ।। ७।।
७. निश्चय ही नियत कर्मों का परित्याग उचित नहीं है; मोहवश उनका परित्याग करना तामसिक कहा गया है।
.....एक अधिक व्यापक दृष्टि से, तथा इन तीनों कार्यों (यज्ञ, दान और तप) को इनके व्यापकतम अर्थ में समझते हुए, जिस कार्य का अनुष्ठान किया जाना है वह है यथोचित रूप से नियंत्रित कर्म, 'नियतं कर्म, अर्थात् वह कर्म जो शास्त्र के द्वारा, समुचित ज्ञान, समुचित कर्म, समुचित जीवनयापन की विद्या एवं कला के द्वारा या मूल स्वभाव के द्वारा नियंत्रित हो, 'स्वभावनियतं कर्म', अथवा अंततः और सबसे श्रेष्ठ रूप में वह कर्म जो हमारे अन्दर और ऊपर अवस्थित भगवान् के संकल्प के द्वारा नियंत्रित हो। इनमें से अन्तिम हो मुक्त पुरुष का वास्तविक तथा एकमात्र कर्म है, मुक्तस्य कर्मी इन कर्मों का परित्याग करना एक उचित वृत्ति नहीं है... इस अज्ञानपूर्ण विश्वास के साथ कर्मों का त्याग कर देना कि सच्ची मुक्ति पाने के लिए ऐसा परित्याग पर्याप्त है, एक तामसिक त्याग है। हम देखते हैं कि कर्मों के त्याग में भी गुण उसी प्रकार हमारा पीछा करते हैं जिस प्रकार कि कर्म-प्रवृत्ति में। अकर्म में आसक्ति रखते हुए, 'संङ्गः अकर्मणि', कमाँ का त्याग करना भी उसी प्रकार एक तामसिक त्याग होगा।
सच्चे कर्म तो वे हैं जो सहज रूप से भगवान् के प्रीत्यर्थ किए जाते हैं, जिन्हें कि मुक्तस्य कर्म कहा जाता है और जो मनुष्य को चेतना को परमात्मा की चेतना की ओर ले जाते हैं और उसके साथ जोड़ देते हैं।
प्रश्न : नियत कर्मों का क्या अर्थ है?
उत्तर : नियत कर्म वे कर्म हैं जो व्यक्ति की श्रद्धा के द्वारा तय किये गए लक्ष्य के अनुरूप नियत होते हैं। उदाहरण के लिए, जब श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति एक गुरु अपनाता है तो उसके नियत कर्म हैं गुरु की सेवा और उनकी आज्ञापालन। इन कर्मों का शिष्य परित्याग नहीं कर सकता। गुरु के प्रीत्यर्थ कर्म करना ही अब उसका धर्म बन जाता है और वही उसके लिए नियत कर्म है। इसमें शिष्य के लिए यज्ञ, तप और दान के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म तो रहते ही नहीं। शिष्य अपनी सभी ऊर्जाओं और बहिर्गामी इंद्रियों को संयमित करने का तप करता है, उन्हें गुरु सेवा में नियोजित करने का दान करता है और कर्मों को गुरु की प्रसन्नता के निमित्त करने का यज्ञ करता है। इस प्रकार साधक के संपूर्ण जीवन को सारी क्रियाएँ यज्ञ, तप और दानस्वरूप होती हैं। सामान्य जीवन में भी वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करके उसमें नियोजित करता है। जितना ही वह अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ रहता है उतनी ही शीघ्र और अधिक सफलता उसे प्राप्त होती है। वहीं, जो उसमें व्यय होने वाले श्रम, ऊर्जा, साधन आदि से सकुचाता है या उसमें प्रमाद करता है वह कभी भी समुचित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः श्रद्धा से जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तब उसी के अनुरूप कर्म भी नियत होते हैं और उन्हें न करना तामसिक वृत्ति या तामसिक त्याग है।
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ।। ८॥
८. जो कर्मों का परित्याग इसलिए करता है क्योंकि वे दुःख के कारक हैं अथवा कायाक्लेश के भय से परित्याग करता है वह राजसिक त्याग करता है और इस प्रकार राजसिक त्याग करने के कारण त्याग के फल को नहीं प्राप्त करता।
यह बौद्धिक निराशावाद अथवा प्राणिक क्लान्ति का परिणाम है; इसका मूक अहंकार में है। ऐसे त्याग से कोई मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती जो इस स्व-केंद्रित या अहंमूलक भाव से शासित हो।
प्रश्न : क्या राजा भर्तृहरि के त्याग को राजसिक त्याग कहा जाएगा?
उत्तर : भर्तृहरि के त्याग में निराशा या फिर जीवन के प्रति विरक्ति का भाव अवश्य था परंतु वे अपने राजकार्य में आवश्यक श्रम से निवृत्त सहने के लिए त्याग नहीं कर रहे थे। राजकार्य का निर्वाह तो वे बहुत ही हसता से कर रहे थे। परन्तु जब उन्होंने देखा कि जिसकी प्रसन्नता है। निमित्त वे अपने कार्य कर रहे हैं वह उस योग्य नहीं है तब उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ।
एक सच्चे दृष्टिकोण से देखा जाए तो त्याग और वैराग्य आदि शब्द तो संसार जिस प्रकार का है उसके प्रति हमारी अतिशय आसक्ति को ही दशति हैं। जब व्यक्ति को अपने बाहरी स्वरूप में यह संसार बहुत ही महत्त्वपूर्ण लगता है तभी वैराग्य या त्याग जैसी भावनाएँ आती हैं। अन्यथा यदि व्यक्ति को गहरे विषयों में, अपनी आंतरिक सत्ता में आनन्द की अनुभूति हो रही हो तब ऐसे में तो त्याग आदि की कोई भावना आ ही नहीं सकती। किसी पत्थर के बदले यदि किसी को बहुमूल्य मणि की प्राप्ति हो रही हो तब इसमें किसी प्रकार के त्याग का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। एक सच्ची चेतना में रहने पर तो व्यक्ति को उत्तरोत्तर प्रगति के साथ अधिकाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। सच कहें तो उस चेतना में रहने वाले व्यक्ति को तो वे लोग त्यागी या दरिद्र प्रतीत होते हैं जो आत्मा की निधियों को छोड़कर क्षणभंगुर चीजों के पीछे निरर्थक ही भटकते रहते हैं और थोड़े से लाभ के लिए जीवन भर भारी मूल्य चुकाते रहते हैं। ज्यों-ज्यों आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ता है त्यों ही त्यों भगवान् उस पर अधिकाधिक अपनी शक्तियों का, अपनी कृपा, चेतना, ज्ञान आदि निधियों का वर्षण करते हैं और व्यक्ति इस पार्थिव सीमितता से मुक्त हो व्यापकता में निवास करने लगता है। तो ऐसे में किसी प्रकार के त्याग की कहाँ संभावना है। इसी कारण आध्यात्मिक पथ के एक साधक को हम भगवान् के प्रति गहरी कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ पाते हैं क्योंकि उसे अनुभव होता है कि भगवान् उसे जब-जहाँ और जिस चीज की आवश्यकता होती है वह स्वयमेव ही प्रदान कर देते हैं और हर चीज में उनकी कृपा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। व्यक्ति ऐसी उच्च चेतना और स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ एक व्यापक दृष्टि से वह चीजों को देख और विचार सकता है। जहाँ पहले वह छोटी-छोटी कामनाओं से सारे दिन प्रताड़ित रहता था, अज्ञान के अंधकार से पीड़ित रहता था, क्षुद्र चेतना में सीमित हो यंत्रणा से गुजर रहा होता था वहीं जब वह चेतना में आरोहण करता है तब भगवान् उसे इन सभी चीजों से मुक्त कर देते हैं और अपने आनंद से सराबोर कर देते हैं। ऐसे में कृतकृत्य होने के अतिरिक्त तो अन्य कोई भाव रहता ही नहीं। इसीलिए यदि वास्तव में व्यक्ति मार्ग पर है तो कभी उसे त्याग का अनुभव नहीं हो सकता। जिन्चे अभी उस अवस्था का अनुभव नहीं है और जो अभी भी उन्हीं भोगों में क्षुद्र ऐंद्रियक सुखों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें संभवतः एक साधक त्यागी प्रतीत हो सकता है परंतु यदि स्वयं साधक को यह त्याग प्रतीत होता है तो यह उसके पथ पर न होने की एक अचूक निशानी है।
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९॥
९. हे अर्जुन! जब व्यक्ति कर्तव्यं कर्म के भाव से, कर्म के प्रति और कर्मफल में आसक्ति का परित्याग करके नियत कर्म करता है, उस त्याग को सात्त्विक माना जाता है।
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।। १० ।।
१०. सत्त्वगुण से पूर्ण रूप से संपन्न और संशयरहित बुद्धिमान् त्यागी का अप्रिय कर्म के प्रति कोई द्वेष नहीं होता और प्रिय या रुचिकर कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती।
किसी प्रिय, काम्य, लाभजनक या सौभाग्यप्रद कर्म के प्रति अवश्य ही कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए और उस कर्म को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका ऐसा (अनुकूल, रुचिकर) स्वभाव है; किन्तु इस प्रकार का कर्म भी तब करना ही होगा, - पूर्ण रूप से, निःस्वार्थ भाव से तथा आत्मा की सहमति के सहित करना होगा, - जब वह ऐसा कर्तव्यं कर्म हो जिसे करने की माँग हमारे ऊपर तथा अन्दर से की जाती हो। किसी अप्रिय, अकाम्य या अतृप्तिकर कर्म के प्रति या जो कर्म अपने साथ दुःख, विपदा, विषम अवस्थाएँ एवं अनिष्ट परिणाम लाता है या ला सकता है उसके प्रति कोई घृणा नहीं होनी चाहिए; क्योंकि वह भी जब एक कर्तव्यं कर्म हो, तब उसे भी पूर्ण रूप से, निःस्वार्थ भाव से तथा उसकी आवश्यकता एवं प्रयोजन को गहराई के साथ समझते हुए अंगीकार करना होगा। ज्ञानी मनुष्य काम-पुरुष की जुगुप्साओं तथा दुविधाओं तथा उस साधारण मानवीय बुद्धि के संशयों को दूर हटा देता है जो क्षुद्र व्यक्तिगत, रूढ़ या फिर सीमित मानदंडों के द्वारा आँकती है।
न हि देहधृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।। ११ ।।
११ . का पूर्णतया परित्याग करना संभव ही है; निश्चय ही जो कर्मफल का त्याग करता है उसे ही त्यागी कहा जाता है।
त्याग का, सच्चे त्याग, सच्चे संन्यास का मूल अर्थ कोई कर्मत्याग या निष्क्रियता का निर्देश नहीं है, अपितु वह है निष्काम आत्मा, निःस्वार्थ मन, तथा अहंभाव से हट कर मुक्त निर्व्यक्तिक एवं आध्यात्मिक प्रकृति में अवस्थित होने का विधान। आंतरिक त्याग का यह भाव ही सात्त्विक साधना की उच्चतम परिणति की सर्वप्रथम मानसिक स्थिति है।
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ।। १२ ।।
१२. कर्म का त्रिविध फल होता है, प्रिय, अप्रिय और मिश्र, जो उन लोगों के लिए मृत्यु के बाद भी बना रहता है जिन्होंने त्याग नहीं किया है; यह कर्मफल उनके लिए कभी नहीं बना रहता जिन्होंने त्याग कर दिया है।
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ।। १३।।
१३. हे महाबाहो ! समस्त कर्मों के संसिद्ध होने के लिये सांख्य सिद्धान्त में कहे गये इन पाँच कारणों को मुझ से जान।
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ।। १४।।
१४. ये हैं आधार, कर्त्ता, विभिन्न करण, अनेक प्रकार की चेष्टाएँ, और पाँचवा, दैव, भाग्य।
आधार, कर्ता, विभिन्न करण, चेष्टाएँ, और दैव इन सब को कर्म का निमित्त कारण कहा गया है क्योंकि वास्तव में कर्म केवल माँ जगदम्बा निरम ही निर्धारित होते हैं। प्रत्येक कर्म के पीछे एकमात्र वे ही कत्री है। भगवान् श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन को ग्यारहवें अध्याय में कहा कि 'निमिरी हैं। भव सव्यसाचिन्'। हमारा कर्ता का भाव, हमारी चेष्टाएँ आदि सब केवल निमित्त हैं। यह निमित्त मात्र होने का भाव भी केवल मानसिक चेतना ये ही महसूस होता है, पशुओं को इसका कोई भान नहीं होता। हमारी मानसिक चेतना का गठन इस प्रकार का है कि हमें कर्तापन का बोध होता है। अतः उपर्युक्त पाँच तत्त्व केवल निमित्त का ही गठन करते हैं न कि परिणाम का। परिणाम तो माँ जगदम्बा के द्वारा ही निर्धारित होता है।
प्रश्न : अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, और दैव, इन पाँचों को हम किस रूप में समझ सकते हैं?
उत्तर : पहला है अधिष्ठान अर्थात् मानव देह, प्राण और मन का ढाँचा जो कि सभी का भिन्न-भिन्न है। यदि किन्हीं जुड़वाँ बच्चों की देह एक जैसी भी हो तो भी उनका मन, प्राण का ढाँचा सर्वथा भिन्न-भिन्न होता है जिसके कारण एक ही प्रकार की क्रिया भी दोनों भिन्न-भिन्न रूप से करेंगे। दूसरा है कर्ता अर्थात् यह भान कि व्यक्ति कर्म कर रहा है। कर्तापन के भाव के भी अनेक स्तर हैं। मनुष्य का अहं जितना ही स्थूल होगा उतना ही अधिक दुःख-दर्द और परिश्रम उसे कार्य में महसूस होगा। वहीं यदि अहं स्थूल न रहकर सूक्ष्म हो गया है, तो कार्य का स्वरूप भी तब उतना स्थूल रूप से अहमात्मक नहीं रहेगा। यह कर्त्तापन का भाव भी एक मनोवैज्ञानिक चीज है। तीसरा है, उपकरण अर्थात् वे विभिन्न करण या साधन – जैसे कि बुद्धि, संकल्प, अध्यवसाय आदि मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ - जिनकी सहायता से कर्म किया जाता है। इसके बाद चौथा तत्त्व है चेष्टा अर्थात् संकल्प की प्रगाढ़ता। यह एक सामान्य तथ्य है कि व्यक्ति को किसी कार्य की भली-भाँति समझ हो और उसके विषय में सारी जानकारी भी हो, परंतु यदि चेष्टा ही न हो तो वह कार्य साधित नहीं होता। और अंतिम तत्त्व है दैव अर्थात् वे सभी शक्तियाँ जो मनुष्य के सीवित सामर्थ्य के वश में नहीं हैं। यदि मनुष्य उन शक्तियों के संपर्क में आकर उन्हें अपने जीवन में सक्रिय कर सके तो इनकी सहायता से अप्रत्याशित कार्य कर सकता है। बिना हमारे इनके विषय में सचेतन हुए भी इनका क्योंकि आखिर इन उच्चतर शक्तियों के हस्तक्षेप के द्वारा माँ जगदम्बा अमारे भीतर परमात्मा का संकल्प साधित करती हैं। इस प्रकार ये सारे हात मिला कर निमित्त बनते हैं। और वास्तव में संसिद्ध वही होता है जो भगवान् द्वारा नियत होता है। ये पाँचों ही तत्त्व मनोवैज्ञानिक हैं। गीता में भगवान् इनका अब विस्तार से वर्णन करेंगे।
__________________
* ये पाँच इस प्रकार हैं, पहला 'अधिष्ठान', अर्थात् देह, प्राण और मन का ढाँचा जो प्रकृति के अन्दर जीव का आधार या अवस्थानभूमि है, उसके बाद है 'कर्ता', तीसरा है 'करण', अर्थात् प्रकृति के विविध उपकरण, चौथा है 'चेष्टाः', अर्थात् अनेक प्रकार के प्रयत्न जो कर्म-शक्ति का गठन करते हैं, और अंतिम है 'दैवम्' या दैव, अर्थात् मानवीय कर्तृत्व से, प्रकृति की गोचर कर्म-पद्धति से भिन्न शक्ति या शक्तियों का प्रभाव, वे शक्तियाँ इनके पीछे रहकर कर्म को संशोधित करती हैं तथा कर्म और कर्मफल के नियमानुसार फल का विधान करती हैं। इन पाँच तत्त्वों के परस्पर-संयोगों से ही कर्म के सब निमित्त-कारण गठित होते हैं; इस प्रकार, मनुष्य अपने मन, शरीर और वाणी से जो कोई भी कर्म करता है उसका रूप-स्वरूप और परिणाम इन्हीं के द्वारा निर्धारित होते हैं।
शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ।। १५।।
१५. शरीर, वाणी और मन के द्वारा मनुष्य उचित अथवा अनुचित जो भी कर्म प्रारम्भ करता है उसके ये पाँच निमित्त कारण होते हैं।
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ।। १६।।
१६. परंतु वस्तुस्थिति ऐसी होने पर भी जो मनुष्य अज्ञानमय बुद्धि होने के कारण केवल अपने-आप को (अपने व्यक्तिगत अहं को) ही कर्ता जानता है वह दुर्मति (विकृत बुद्धि वाला) मनुष्य यथार्थ नहीं देखता।
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।। १७।।
१७. जो स्वयं कर्ता होने के अहंभाव से मुक्त है, जिसकी बुद्धि (कर्मफल में) अलिप्त है, वह इन सब मनुष्यों को मारकर भी नहीं मारता और न कर्म से बद्ध होता है।
जब हम अहं से मुक्त हो जाते हैं तब हमारी पीछे अवस्थित सच्ची आत्मा, निर्व्यक्तिक और विश्वगत आत्मा सामने आ जाती है, और विश्वात्मा के साथ अपने एकत्व की आत्म-दृष्टि में वह विश्व-प्रकृति को कर्म की कर्ती के रूप में और उसके पीछे अवस्थित भगवत्संकल्प को विश्व-प्रकृति के स्वामी के रूप में देखती है। जब तक हमें यह ज्ञान नहीं प्राप्त होता केवल तभी तक हम अहं के ऐसे स्वरूप से और कत्र्तापन के उसके संकल्प से बंधे होते हैं और शुभाशुभ कर्म करते तथा अपनी तामसिक, राजसिक या सात्त्विक प्रकृति की तुष्टि प्राप्त करते हैं। परन्तु एक बार जब हम इस महत्तर ज्ञान में वास करने लगते हैं तब कर्म के स्वरूप और उसके फल या परिणाम से आत्मा के स्वातंत्र्य में कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। बाहर से वह कर्म कुरुक्षेत्र के इस महान् युद्ध और संहार जैसा घोर कर्म हो सकता है; परन्तु मुक्त पुरुष उस संघर्ष में भाग भले ही लेता है और इन सब प्रजाओं का भले ही वध भी करता है, फिर भी वह किसी का वध नहीं करता और अपने कर्म से बद्ध नहीं होता, क्योंकि वह कर्म सर्वलोकमहेश्वर का होता है और उन्होंने अपने गुप्त सर्वशकिीता, संकल्प में पहले से ही इन सब सेनाओं का वध कर रखा होता है... मुरा पुरुष विश्वात्मा से एकात्म हो जीवंत यंत्र की भाँति अपने नियुक्त कार्य को संपन्न करता है।... उसे इस बात का ज्ञान होता है कि पराशक्ति ही उसके संपन्नग्राण-शरीररूपी आधार, 'अधिष्ठान', के अन्दर एकमात्र कर्ती के रूप में दैव-नियत कर्मों को संपन्न कर रही है, और वह दैव वास्तव में दैव, कोई यांत्रिक कर्म-विधान नहीं अपितु एक ज्ञानमय सर्वदर्शी संकल्प है जो मानव-कर्म के पीछे क्रियारत है.....
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्म ही एकमात्र महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है; जिस ज्ञान के आधार पर हम कर्म करते हैं उसके कारण आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक अन्तर आ जाता है। गीता कहती है कि तीन चीजें हैं जो कमाँ की मानसिक प्रेरणा का गठन करती हैं...
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ।। १८ ।।
१८. ज्ञान, ज्ञेय विषय और ज्ञाता, ये तीन कर्म में प्रवृत्त करनेवाले तत्त्व हैं: कर्ता, उपकरण, और किया जाने वाला कर्म, ये तीनों कर्म को एक साथ संगृहीत करते हैं (और उसे संभव बनाते हैं)।
सात्त्विक मन, जो सदैव उचित समस्वरता और उचित ज्ञान की खोज करता है, सात्त्विक मनुष्य का प्रधान उपकरण या साधन होता है और शेष सारे यंत्र को चलाता है। कामना-पुरुष के द्वारा समर्थन-प्राप्त अहंमय काम-संकल्प राजसिक कर्मी का प्रधान करण होता है। भौतिक मन और स्थूल प्राणिक प्रकृति की अज्ञ सहजवृत्ति या अनालोकित प्रवृत्ति तामसिक कर्मी की मुख्य करण-शक्ति है। मुक्त व्यक्ति का साधन होती है एक महत्तर आध्यात्मिक ज्योति और शक्ति जो उच्चतम सात्त्विक बुद्धि से कहीं अधिक उच्चतर है, और वह उसके अन्दर पराभौतिक केंद्र से एक परिव्याप्त करने वाले अवतरण के द्वारा कार्य करती है तथा पवित्रीकृत और ग्रहणशील मन, प्राण और शरीर को अपनी शक्ति की निर्मल वाहिका के रूप में प्रयोग करती है।
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिचैव गुणभेदतः ।
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ।। १९।।
१९. सांख्य कहता है कि ज्ञान, कर्म और कर्त्ता गुण-भेद के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं; उन्हें भी तू यथावत् सुन।
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ।। २० ।।
२०. जिस ज्ञान के द्वारा (मनुष्य) समस्त भूतों में एक अविनाशी सत् को, समस्त विभक्त पदार्थों में एकतम अविभक्त को, देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान।
सात्त्विक ज्ञान.... अस्तित्व को इन सब विभाजनों के अन्दर एक ही अविभाज्य समग्र, सभी भूतभावों के अन्दर एक ही अविनाशी सत्ता के रूप में देखता है: यह उसके कर्म के विधान को तथा सत्ता के समग्र उद्देश्य के साथ किसी विशिष्ट कर्म के सम्बन्ध को अधिकृत करता है; यह संपूर्ण प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम, प्रत्येक चरण को उसके समुचित स्थान में सुव्यवस्थित करता है। ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर यह दृष्टि जगत् में, इन सब अनेकानेक भूतों में अवस्थित एक आत्मा का, सब कर्मों के एक ही स्वामी का ज्ञान बन जाती है, यह ज्ञान बन जाती है कि विश्व की शक्तियाँ भगवान् की ही अभिव्यक्तियाँ हैं और स्वयं कर्म भी मनुष्य, उसके जीवन एवं मूल स्वभाव में होनेवाली उनके परम संकल्प और ज्ञान की क्रियाएँ हैं। व्यक्तिगत संकल्प पूर्ण रूप से सचेतन, ज्ञानदीप्त, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हो जाता है, और वह एकमेव में निवास करने तथा कर्म करने और उनके परम आदेश की उत्तरोत्तर पूर्णता के साथ अनुपालना करने लगता है, मानव-रूप में उनकी ज्योति और शक्ति का एक अधिकाधिक निर्दोष यंत्र बनता जाता है। सात्त्विक ज्ञान की इस पराकाष्ठा के द्वारा ही परमोच्च मुक्त कर्म की स्थिति आती है।
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ।। २१ ।।
२१. जो ज्ञान विविध प्रकार के पदार्थों को केवल पृथक-पृथक् ही देखता है और समस्त भूतों में केवल पृथक् पृथक् व्यापारों को देखता है उस ज्ञान को तू राजसिक जान।
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् ।
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ।। २२।।
२२. जबकि, जो (ज्ञान) क्षुद्र है और किसी एक कार्य को बिना किसी कारण के, बिना तत्त्वतः उसका अर्थ जाने ही ऐसे पकड़ लेता है मानो वही समय या सब कुछ हो, उसे तामसिक कहा गया है।
------------------------------------------------
* यह जानना ज्ञान के, प्रायः विश्रृंखल ज्ञान के कुछ ऐसे खंडों का अस्तव्यस्त मिश्रण होता है जिन्हें मन हमारे अर्द्ध-ज्ञान और अर्द्ध-अज्ञान के संभ्रम में से किसी प्रकार का रास्ता बनाने के लिए बलपूर्वक संयुक्त किये होता है। या फिर यह एक चंचल राजसिक बहुविध क्रिया होती है जिसमें न तो कोई स्थिर नियामक उच्चतर आदर्श होता है और न ही ज्योति और शक्ति का कोई विवेकी विधान होता है।
तामसिक मन वास्तविक कार्य-कारण की खोज नहीं करता, अपितु अपने-आप को किसी एक क्रिया में या कार्यपरिपाटी में हठपूर्ण आसक्ति के साथ तल्लीन कर देता है, व्यक्तिगत कर्म का जो छोटा-सा भाग उसकी आँखों के सामने होता है उसे छोड़कर वह और कुछ भी नहीं देख सकता और वास्तव में वह यह भी नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, बल्कि अंधे की तरह प्रकृतिगत प्रवृत्ति को उसके कर्म के द्वारा कार्य करने देता है जिसके परिणामों के सम्बन्ध में उसे न कोई कल्पना, न पूर्वदृष्टि या व्यापक समझ हो होती है।....
इसी प्रकार, तीन और चीजें हैं - कर्त्ता, करण (साधन) और कर्म - जो मिलकर किसी कर्म को संगठित करती हैं तथा उसे सम्भव बनाती हैं। यहाँ भी गुणों का भेद ही इन तत्त्वों में से प्रत्येक का स्वरूप निर्धारित करता है।
नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।। २३।।
२३. जो कर्म फल की इच्छा न रखनेवाले व्यक्ति के द्वारा यथावत् नियंत्रित, आसक्ति रहित, राग एवं द्वेष के बिना किया जाता है वह सात्त्विक कहा जाता है।
सात्त्विक कर्म वह है जिसे मनुष्य बुद्धि और ज्ञान के निर्मल प्रकाश में तथा उचित कर्म अथवा कर्तव्य अथवा किसी आदर्श द्वारा अपेक्षित कर्म के निर्वैयक्तिक भाव से शांतचित्तता के साथ सम्पन्न करता है, जिसे ऐसे कर्म के रूप में किया जाता है कि वह करने योग्य है भले ही उस कर्म का उसे इस लोक में या किसी अन्य लोक में कैसा भी फल प्राप्त हो, ऐसा कर्म जो बिना आसक्ति के, कर्म की उत्साही या उबाऊ प्रकृति के प्रति कोई रुचि या अरुचि न रखते हुए, केवल अपनी विचारशक्ति और यथोचितता के बोध की संतुष्टि के लिए तथा सुबोध बुद्धि, प्रबुद्ध संकल्प, शुद्ध निःस्वार्थ मन तथा उच्च तृत आत्मा की संतुष्टि के लिए किया जाता है। सत्त्व की चरम परिणति की सोमा पर यह रूपांतरित होकर एक उच्चतम निवैयक्तिक कर्म बन जाएगा जो पहले की तरह बुद्धि के द्वारा नहीं अपितु हमारी अंतःस्थ आत्मा के द्वारा आदिष्ट होगा, एक ऐसा कर्म जो प्रकृति के परमोच्च धर्म के द्वारा परिचालित होगा, निम्न अहं और उसके हल्के या भारी बोझ से मुक्त होगा, यहाँ तक कि सर्वोत्तम अभिमत, उत्कृष्टतम कामना, शुद्धतम व्यक्तिगत संकल्प या उच्चतम मानसिक आदर्श के सीमाबंधनों से भी विमुक्त होगा। वहाँ इनमें से कोई भी रुकावटें नहीं रहेंगी; इनके स्थान पर प्रतिष्ठित होगा एक सुबोध आध्यात्मिक आत्म-ज्ञान और प्रकाश, कर्म करनेवाली अमोघ शक्ति का तथा जगत् के लिए और जगदीश्वर के लिए किये जाने योग्य कर्म का एक अचूक अंतरंग बोध।
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः ।
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ।। २४।।
२४. किंतु कामना की तुष्टि के लिए, अथवा अहंभाव से और बहुत अधिक (अनियमित) परिश्रम से किया गया कर्म राजसिक कहा गया है।
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।। २५॥
२५. जो कर्म बिना अपनी सामर्थ्य का विचार किये, बिना उसके परिणामों, उससे होने वाली हानि अथवा (दूसरों को होने वाली) क्षति को ध्यान में रखे मोह के वशीभूत होकर आरंभ किया जाता है, उसे तामसिक कहा जाता है।
तामसिक कर्म वह है जो सहज-वृत्तियों, आवेगों और दृष्टिहीन विचारों की यंत्रवत् पालना करते हुए, भ्रमित, मूढ़ या विमोहित और अज्ञानी मन के साथ किया जाता है, और यह सब किया जाता है शक्ति या सामर्थ्य को ध्यान में रखे बिना, अथवा अंधे रूप से दुष्प्रयुक्त प्रयत्न की क्षति एवं हानि का, अथवा आवेग, प्रयास या परिश्रम के पूर्ववर्ती कारण और परिणाम तथा उचित अवस्थाओं का कुछ भी विचार किये बिना।
मुक्तसङ्गोऽनहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः ।
सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ।। २६।।
२६. जो आसक्ति से रहित, अहंभाव से रहित, दृढ़-निश्चयता और उत्साह से युक्त, सफलता और असफलता से अप्रभावित रहता है, वह कर्ता सात्त्विक कहा जाता है।
सात्त्विक कर्ता इस सब आसक्ति, इस अहंभाव, इस उग्र बल या आवेशात्मक दुर्बलता से मुक्त होता है; उसका ऐसा मन एवं ऐसी इच्छाशक्ति होती है जो सफलता से फूल नहीं जाती, विफलता से खिन्न नहीं होती, जो कर्म करना होता है उसमें वह दृढ़ निर्वैयक्तिक संकल्प, शान्त शुद्ध उमा गो उच्च, शुद्ध, निःस्वार्थ उत्साह से पूर्ण होती है। सत्त्व की पराकाष्ठा पर और उसके परे यह संकल्प, उमंग और उत्साह आध्यात्मिक तपस् की सहज किया बन जाते हैं और अन्त में तो ये एक उच्चतम आत्मबल, प्रत्यक्ष भगवत्-रीका, मानव-यंत्र में दिव्य शक्ति की बलशाली और दृढ़-स्थिर गति, द्रष्ट संकल्प एवं विज्ञानमय मनीषा के स्वयं सुनिश्चित पग और इसके साथ ही मुक्त प्रकृति के कर्मों में स्वतंत्र आत्मा का विशाल आनंद बन जाते हैं।
रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।। २७।।
२७. जो आवेशी है, व्याकुलता के साथ कर्मफल की अभिलाषा करता है, लोभी, हिंसात्मक, अपवित्र है, और हर्ष और शोक से चालित होता है, ऐसे कर्ता को राजसिक कहा गया है।
दूसरी ओर, राजसिक कर्त्ता वह होता है जो कर्म में आतुरतापूर्वक आसक्त रहता है, उसे जल्दी से समाप्त करने पर तुला होता है, फल, पुरस्कार और परिणाम के लिए तीव्र रूप से उत्कंठित रहता है, हृदय से लोभी और मन से अपवित्र होता है, जिन साधनों का वह प्रयोग करता है उनमें वह प्रायः उग्र, क्रूर और पाशविक होता है; जब तक उसे अपनी वांछित वस्तु की प्राप्ति होती रहती है, उसकी कामना-वासना की पूर्ति तथा उसके अहं की माँगों का समर्थन होता रहता है तब तक वह इस बात की कुछ परवाह नहीं करता कि वह किसे हानि पहुँचाता है या दूसरों की कितनी क्षति करता है। सफलता में वह हर्ष के मारे फूला नहीं समाता, विफलता में वह बुरी तरह से व्यथित और आहत होता है।
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ।। २८॥
२८. जो विसंगतियों से भरा है, अशिष्ट, ढीठ, धूर्त, दूसरों का बुरा चाहने वाला, विषादयुक्त, आलसी और कर्म में विलंब करने या उसे टालने वाला है, ऐसा कर्त्ता तामसिक कहा जाता है।
तामसिक कर्त्ता वह है जो अपने-आप को वास्तव में कर्म में नहीं लगाता, अपितु एक यांत्रिक मन से कर्म करता है, अथवा साधारण जनता के अत्यंत असंस्कृत विचार का अनुसरण करता है, सामान्य ढर्रे पर चलता रहता है या अंघ भ्रांति और पूर्वाग्रह में अत्यासक्त होता है। वह मूढ़ता पर अड़ा रहता है, अपनी गलती पर हठ करता है और अपने अज्ञानमय कर्म पर मूर्खतापूर्ण गर्व अनुभव करता है; उसके अन्दर संकीर्ण और कुटिल धूर्तता सच्ची बुद्धि का स्थान ले लेती है; जिनसे उसे व्यवहार करना होता है उनके प्रति, विशेषकर अपने से अधिक बुद्धिमान् एवं श्रेष्ठ लोगों के प्रति उसके अन्दर मूढ़ एवं धृष्टतापूर्ण घृणा होती है। जड़तापूर्ण आलस्य, मंदता, कर्म में विलंब या टालने को प्रवृत्ति, शिथिलता, उत्साह या निष्कपटता का अभाव उसके कर्म के लक्षण होते हैं। तामसिक मनुष्य साधारणतः कर्म करने में मंद, अपनी गति में विलंबकारी, सहज ही खिन्न होने वाला, और यदि कोई कार्य उसके सामर्थ्य, प्रबत्न या धैर्य पर जोर डालता है तो उसे शीघ्र ही छोड़ देने के लिए तैयार रहता है।
बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ।। २९ ।।
२९. हे धनञ्जय! बुद्धि का और घृति का गुणों के अनुसार त्रिविध भेद भी पूर्ण रूप में तथा पृथक् पृथक् रूप में सुन।
सज्ञान संकल्प से युक्त बुद्धि एक मानुषी संपदा है और यह मनुष्य के अन्दर जिस रूप में या जितनी मात्रा में होती है उसी के अनुसार उसमें कार्य करती है और उसी के अनुसार ही यह मनुष्य के मन की भाँति यथोचित या विकृत, तमाच्छादित या आलोकित, संकीर्ण और क्षुद्र या विशाल एवं व्यापक होती है। उसकी प्रकृति की मेधा-शक्ति, 'बुद्धि' ही उसके लिए कर्म का चुनाव करती है अथवा बहुधा यह उसकी जटिल सहज-वृत्तियों, आवेगों, विचारों और कामनाओं के अनेक सुझावों में से किसी एक या दूसरे को स्वीकृति प्रदान करती है तथा उसका अनुमोदन करती है। यही उसके लिए उचित या अनुचित, कर्तव्य या अकर्तव्य, धर्म या अधर्म का निर्णय करती है। और 'धृति', अर्थात् संकल्प की दृढ़ता, मानसिक प्रकृति की वह निरंतर शक्ति है जो कर्म को धारण करती तथा उसे संगति और दृढ़ता प्रदान करती है। यहाँ भी त्रिगुण का प्रभाव देखने में आता है।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ।। ३० ।।
३०. हे अर्जुना जो बुद्धि प्रवृत्ति (कर्म करने के विधान को) और निवृत्ति (कर्म से दूर होने के विधान को), करने योग्य कर्म को और न करने योग्य कर्म को, भय और अभय को, बंधन और मुक्ति को तत्त्वतः जानती है, वह सात्त्विक होती है।
विश्व की गति को, प्रवृत्ति (कर्म-विधान) और निवृत्ति (अकर्म-विधान) को, कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म को, जीव के लिए जो निरापद है और जो संकटप्रद है उसे, जिस चीज से भय करने और पीछे हटने की आवश्यकता है उसे और जिस चीज का संकल्प के द्वारा आलिंगन करने की आवश्यकता है उसे, जो वस्तु मनुष्य की आत्मा को बाँधती है और जो उसे बंधन से पुक करती है उसे सात्त्विक बुद्धि उसके उचित स्थान, उचित रूप और उचित मान में देखती है। अपने प्रकाश की मात्रा के अनुसार और उच्चतम पुरुष एवं आत्मा की ओर अपने ऊर्ध्वमुख आरोहण में यह विकास की जिस अवस्था तक पहुँची है उसके अनुसार यह अपने सचेतन संकल्प की दृढ़ता के द्वारा इन्हीं चीजों का अनुसरण या वर्जन करती है। अभीप्साशील बुद्धि जब साधारण तर्कबुद्धि एवं मानसिक संकल्प से परे की वस्तुओं पर स्थिर रूप से एकाग्र हो जाती है, शिखरों की ओर उन्मुख रहती है, इन्द्रियों और प्राण के स्थिर नियंत्रण, मनुष्य की उच्चतम आत्मा, विश्वमय भगवान् एवं विश्वातीत आत्म-तत्त्व के साथ योगयुक्त होने में प्रवृत्त रहती है तब इसकी उस उच्च धृति के द्वारा सात्त्विक बुद्धि की चरम परिणति उपलब्ध होती है। सत्त्वगुण के द्वारा वहाँ पहुँचने पर ही मनुष्य गुणों को पार कर सकता है, मन और उसकी संकल्प-शक्ति एवं बुद्धि की सीमाओं के परे आरोहण कर सकता है और स्वयं सत्त्व भी उस तत्त्व में विलीन हो सकता है जो गुणों के ऊपर तथा इस उपकरणीय प्रकृति के परे है। वहाँ जीव ज्योति में सुप्रतिष्ठित तथा आत्मा, अध्यात्म-सत्ता एवं भगवान् के साथ दृढ़ एकत्व-पद पर आसीन हो जाता है। उस शिखर पर पहुँच कर हम अपने अंगों में दिव्य क्रिया की मुक्त स्वच्छंदता के साथ प्रकृति को परिचालित करने का भार परम देव के ऊपर छोड़ सकते हैं: क्योंकि वहाँ न तो कोई ऐसी दोषपूर्ण या भ्रांत क्रिया होती है और न ही त्रुटि या असमर्थता का कोई ऐसा तत्त्व होता है जो आत्मा की ज्योतिर्मय पूर्णता एवं शक्ति को तमसाच्छन्न या विकृत कर सके। इन सब निम्न अवस्थाओं, निम्न धर्मों का हम पर कोई अधिकार नहीं रहता; अनंत भगवान् मुक्त पुरुष के अन्दर कर्म करते हैं, वहाँ मुक्त आत्मा के अमर सत्य और धर्म के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं होता, कोई कर्म तथा किसी प्रकार का बन्धन नहीं होता।
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।। ३१।।
१९. हे पाथी जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म को और अधर्म को तथा कर्तव्य को और अकर्तव्य को उचित रूप में (ठीक-ठीक) नहीं जानता वह बुद्धि राजसिक होती है।
राजसिक बुद्धि जब भ्रांति और अशुभ के लिए ही भ्रांति और अशुभ का चुनाव जान-बूझ कर नहीं करती तब वह धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य में विभेद कर तो सकती है, पर ऐसा वह सही-सही नहीं अपितु उनके यथार्थ मानों को तोड़-मरोड़ कर तथा उनके मूल्यों को निरन्तर विकृत करके ही करती है और इसका कारण यह है कि इसके तर्क और संकल्प अहं के तर्क और कामना के संकल्प होते हैं और अहंता तथा कामना की ये शक्तियाँ अपने अहंमूलक उद्देश्य की सिद्धि के लिए सत्य और धर्म को अयथावत् निरूपित करती हैं तथा उन्हें विकृत कर देती हैं। जब हम अहं और कामना से मुक्त होकर, केवल सत्य और उसके परिणामों से ही सम्बन्ध रखते हुए शान्त, शुद्ध, निःस्वार्थ मन के द्वारा धीर-स्थिर भाव से वस्तुओं पर दृष्टिपात करते हैं केवल तभी हम उन्हें सही रूप से तथा उनके यथार्थ मूल्यों सहित देखने की आशा कर सकते हैं। परन्तु राजसिक संकल्प-शक्ति अपने स्वार्थ एवं सुख का और जिसे वह धर्म एवं न्याय समझती है या समझना पसंद करती है उसका अनुसरण करती हुई अपनी आसक्तिपूर्ण आकांक्षाओं एवं कामनाओं की तृप्ति पर ही अपना ध्यान दृढ़तापूर्वक लगाये रहती है। इसकी प्रवृत्ति सदा इसी ओर होती है कि इन चीजों को ऐसा रूप दे दे जो इसकी अपनी कामनाओं की सर्वाधिक चापलूसी तथा समर्थन करनेवाला हो और साथ ही, जो साधन इसे अपने कर्म और प्रयत्न का वांछित फल प्राप्त करने में सर्वोत्तम रूप से सहायता देते हों उन्हें यथार्थ या समुचित ठहराए। मानवीय बुद्धि और संकल्प के संपूर्ण असत्य और अनाचार में से तीन-चौथाई का कारण यही है। प्राणिक अहं पर प्रबल आधिपत्य रखनेवाला रजस् महान् पापी और सुनिश्चित कुमार्गदर्शक है।
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।
सर्वार्थान्विपरीतांश्व बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।। ३२।।
३२. हे पार्थ। अंधकार से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म समझती है और समस्त पदार्थों को विपरीत या विकृत रूप में समझती है वह तामसी होती है।
तामसिक तर्कबुद्धि एक मिथ्या, अज्ञानी और तमसाच्छन्न उपकरण होती है जो हमें सब चीजों को मंद और दोषपूर्ण प्रकाश में, कुधारणाओं के कुहासे में देखने के लिए तथा वस्तुओं और व्यक्तियों के महत्त्व की मूर्खतापूर्वक उपेक्षा करने के लिए बाध्य कर देती है। यह बुद्धि प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश कहती है, जो सच्चा धर्म नहीं है उसे ले लेती है और उसे ही धर्म के रूप में थामे रखती है, जिस कार्य को करना उचित नहीं उसमें रत रहती है और हमारे सामने उसका एकमात्र करने योग्य उचित कार्य के रूप में समर्थन करती है। इसका अज्ञान अपराजेय है और इसकी धृति या संकल्पगत दृढ़ता अपने अज्ञान की संतुष्टि एवं उसके जड़ अहंकार को दृढ़ता से पकड़े रहने में ही है। यह सब तो इसकी अंध क्रिया का पहलू है; परंतु इसके साथ ही लगा रहता है जड़ता और अशक्तता का भारी दबाव, मंदता और निद्रा में दृढ़ स्थिति, मानसिक परिवर्तन और उन्नति के प्रति अरुचि, जो भय, शोक और विषाद हमारी प्रगति को रोकते हैं अथवा हमें हीनता, दुर्बलता और कायरता से भरे मार्गों में ही फँसाये रखते हैं उनके विषय में मन की संलग्नता। तामसिक संकल्प और बुद्धि के लक्षण हैं - भीरुता, कातरता, छल-चातुरी, अलसता, अपने भयों, मिथ्या संदेहों, सतर्कताओं एवं कर्त्तव्य-विमुखताओं का और हमारी उच्चतर प्रकृति की पुकार से च्युति एवं पराङ्गमुखता का मन के द्वारा समर्थन, न्यूनतम प्रतिरोधवाली दिशा का सुरक्षित अनुसरण जिससे कि हमें अपने परिश्रम का फल अर्जित करने में कष्ट, क्लेश और संकट कम-से-कम हो, - यह कहती है कि चाहे कोई भी फल न मिले या केवल कोई अति तुच्छ फल ही मिले पर कोई महान् एवं श्रेष्ठ पुरुषार्थ या कठोर एवं संकटपूर्ण परिश्रम और साहस-कार्य न करना पड़े।
धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः ।
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ।। ३३।।
३३. हे पार्थ! जिस अडिग धृति से, योग के द्वारा, व्यक्ति मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वह धृति सात्त्विक होती है।
यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ।
प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी घृतिः सा पार्थ राजसी ।। ३४ ।।
३४. हे अर्जुना जिस घृति से मनुष्य तीव्र आसक्ति के साथ फल की कामना करता हुआ धर्म, अर्थ और काम में स्थिरता से प्रवृत्त होता है, हे पाथी वह धृति राजसिक होती है।
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।
न विमुञ्श्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ।। ३५।।
३५. हे पार्थ। जिस घृति से विपरीत या विकृत बुद्धिवाला मनुष्य निद्रा, भय, हिंता, शोक, और अभिमान को भी नहीं छोड़ता है, वह धृति तामसिक होती है।
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।। ३६।।
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ।। ३७।।
३६-३७. हे भरतश्रेष्ठा अब तू मुझसे त्रिविध सुख के विषय में सुन। जिस सुख में मनुष्य अभ्यास के द्वारा रमण करता है और जो दुःख-कष्ट का अंत कर देता है, जो प्रारंभ में विष के समान होता है परंतु अंत में अमृत के समान होता है, आत्मा के सुस्पष्ट ज्ञान से उत्पन्न वह सुख सात्त्विक कहा जाता है।
सात्त्विक मन और स्वभाव के विशिष्ट गुण होते हैं सामंजस्य और सुव्यवस्था, निश्चल सुख, एक विशद और शांत संतोष और एक आंतरिक विश्राम और शांति... यह सुख बाह्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, अपितु एकमात्र हमारे अपने ऊपर और हमारे अंदर जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ तथा अंतरतम है उसके कुसुमित होने के ऊपर निर्भर करता है। परंतु आरंभ में यह सुख हमारी सामान्य संपदा नहीं होता; इसे आत्म-अनुशासन के द्वारा, आत्मा के पुरुषार्थ के द्वारा और उच्च एवं कठोर प्रयास के द्वारा अर्जित करना होता है। आरंभ में इसका अर्थ होता है अभ्यस्त सुख की अत्यधिक हानि, बहुत अधिक कष्ट और संघर्ष, हमारी प्रकृति के मंथन से उत्पन्न विष, शक्तियों का एक दुःखदायी संघर्ष, हमारे अंगों की दुष्प्रवृत्ति या प्राणिक चेष्टाओं के दुराग्रह के कारण परिवर्तन के प्रति अत्यधिक विद्रोह और विरोध, परंतु अंत में इस कटुता के स्थान पर अमृतत्व की सुधा उद्भूत होती है और जैसे-जैसे हम उच्चतर आध्यात्मिक प्रकृति की और आरोहण करते जाते हैं वैसे-वैसे हमारे दुःख का अंत होता जाता है, शोक-संताप का अनायास ही लोप होता जाता है। यही वह सर्वातिशयी सुख है जो सात्त्विक साधना की परिणति के चरम बिंदु या सीमा पर हमारे ऊपर उतर आता है।
सात्त्विक प्रकृति का आत्म-अतिक्रमण केवल तभी साधित होता है जब हम महान् पर अभी भी अपेक्षाकृत हीन सात्विक सुख से परे, मानसिक ज्ञान और पुण्य एवं शांति से मिलनेवाले सुखों से परे जाकर आत्मा की शाश्वत शांति और दिव्य एकत्व का आध्यात्मिक परमानंद प्राप्त कर लेते हैं। वह आध्यात्मिक सुख अब और अधिक सात्त्विक 'सुख' नहीं रहता अपितु परम आनंद हो जाता है। आनंद ही वह गुप्त तत्त्व है जिससे सब वस्तुएँ उत्पन्न हुई है. जिसके द्वारा सब वस्तुएँ अस्तित्व में बनी रहती हैं और जिसकी ओर वे अपनी आध्यात्मिक परिणति में ऊपर उठ सकती हैं। उस आनंद की उपलब्धि की तभी हो सकती है जब मुक्त व्यक्ति अहंकार और उसकी कामनाओं से मुक्त होकर अंततः अपनी उच्चतम आत्मसत्ता से सर्व भुता से तथा परमेश्वर से एकीभूत होकर आत्मा के पूर्णतम आनंद में निवास करता है।
नित्रैगुण्य की अवस्था में सदा ही पूर्णतम आनंद होता है। सात्विक अवस्था में कर्म से पहले परिश्रम या दुःख होता है परंतु अंततः आनंद या सुख प्राप्त होता है, राजसिक अवस्था में पहले सुख का अनुभव होता है परंतु परिणाम दुःखांत होता है, वहीं तामसिक अवस्था में पहले भी दुःख होता है और बाद मेंभी दुःख होता है।
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे ऽमृतोपमम् ।
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ।। ३८।।
३८. जो सुख इन्द्रियों के उनके विषयों के साथ संयोग से उत्पन्न होता है, प्रारंभ में अमृत के समान प्रतीत होता है, परंतु अंत में विष के समान होता है वह सुख राजसिक कहा गया है।
राजसिक मनुष्य का मन एक अधिक उग्र अथवा तीक्ष्ण और मादक प्याले का रसास्वादन करता है; शरीर और इंद्रियों का तथा इंद्रियासक्त या प्रचंड रूप से गतिमय संकल्प एवं बुद्धि का तीव्र, चंचल एवं सक्रिय सुख हो उसके लिए जीवन का समस्त आनंद और जीवन-धारण का वास्तविक अर्थ होता है। प्रथम स्पर्श में तो यह सुख अधरों के लिए सुधामय होता है, परंतु प्याले के तल में एक प्रच्छन्न विष रखा होता है और पीने के बाद इसका परिणाम होता है निराशा की कटुता, वितृष्णा, क्लान्ति, विद्रोह, जुगुप्सा, पाप, यातना, हानि, अनित्यता। और ऐसा होना अनिवार्य ही है क्योंकि इन सुखों के बाह्य रूप वे चीजें नहीं हैं जिन्हें हमारी अंतरस्थ आत्मा सचमुच में जीवन से प्राप्त करना चाहती है; बाह्य रूप की नश्वरता के पीछे और परे भी कोई चीज है; कोई चिरस्थायी, संतोषप्रद और स्वतः-पर्याप्त वस्तु भी है।
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ।। ३९।।
३९. और जिस सुख से जीव प्रारंभ में और अंत में विमोहित रहता है और और प्रमाद से उत्पन्न होता है उसे तामसिक कहा गया है ।
प्रकृति ने इसे [तामसिक अहंकार को] मूढ़ता और अज्ञानता में, गुहा के पेट प्रकाशों, जड़ संतोष, इसके क्षुद्र या निकृष्ट हर्षों और इसके भद्दे सुखों में ही एक उत्सुक संतुष्टि पाने का विशेष सौभाग्य प्रदान किया है। भ्रांति ही इस सुख-संतोष का आरंभ है और मोह-भ्रांति ही इसका परिणाम है; परंतु फिर भी गुहा के निवासी को अपनी मोह-भ्रांतियों में एक मंद-निस्तेज सुख प्राप्त रहता है जो किसी भी प्रकार सराहनीय न होते हुए भी उसके लिए यथेष्ट होता है। तमस् या जड़ता और अज्ञान में एक तामसिक सुख आधारित है।
II. स्वभाव और स्वधर्म
सामान्य स्तर पर समस्त कर्म त्रिगुण के द्वारा निर्धारित होता है; करने योग्य कर्म, 'कर्तव्यं कर्म', दान, तप और यज्ञ का त्रिविध रूप ले लेता है, और इन तीन में से कोई भी एक या ये सभी किसी भी गुण का स्वभाव धारण कर सकते हैं। अतएव हमें इन चीजों को इनके सामर्थ्यानुसार उच्चतम संभव सात्त्विक शिखर तक ऊँचा उठाते हुए ही आगे बढ़ना होगा और फिर उस शिखर से और भी परे एक ऐसी विशालता की ओर जाना होगा जिसमें सभी कर्म एक मुक्त आत्म-दान, दिव्य तपस् की एक शक्ति, आध्यात्मिक जीवन का एक नित्य यज्ञ बन जाते हैं। परंतु यह एक सर्वसामान्य नियम है और इन सब विवेचनों के द्वारा सर्वथा व्यापक सिद्धांतों की ही व्याख्या की गयी है, ये सब कर्मों और सब मनुष्यों पर समान रूप से, बिना किसी भेदभाव के लागू होते हैं। आध्यात्मिक विकास के द्वारा अंत में सभी इस प्रबल अनुशासन, इस व्यापक पूर्णता, इस उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति तक पहुँच सकते हैं। परंतु जहाँ मन और कर्म का सर्वसाधारण नियम सभी मनुष्यों के लिए एक-सा है, वहाँ हम यह भी देखते हैं कि वैविध्य का भी एक शाश्वत नियम है और प्रत्येक व्यक्ति मानवीय आत्मा, मन, संकल्प-शक्ति और प्राण के सार्वभौम नियमों के अनुसार ही नहीं अपितु अपनी प्रकृति के अनुसार भी कर्म करता है; प्रत्येक मनुष्य अपनी परिस्थितियों, क्षमताओं, प्रवृत्ति, चरित्र एवं शक्ति-सामर्थ्य के नियम के अनुसार विभिन्न कर्तव्यों को पूर्ण करता या विभिन्न दिशा का अनुसरण करता है। अध्यात्म-साधना में इस वैविध्य को, प्रकृति के इस व्यक्तिगत नियम को क्या स्थान देना चाहिए?
यहाँ श्रीअरविन्द इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि आखिर गीता में स्वभाव की चर्चा ही क्यों आई है। सभी मानवों के एक सामान्य गतिक्रम में प्रत्येक व्यक्ति पहले तमस् से रजस् की ओर, फिर रजस् से सत्त्व की ओर और अंततः सत्त्व से निलैगुण्य की ओर आरोहण करेगा। हालाँकि इस सामान्य गतिक्रम में भी सदा ही यह संभावना रहती है कि कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था से सीधे ही निखैगुण्य की स्थिति में जा सकता है। यह तो एक ऐसा अप्रत्याशित विधान है जिसकी सदा ही संभावना तो रहती है परंतु यह कोई सामान्य क्रम नहीं है। सामान्य क्रम तो गीता में वर्णित तमस्, रजस् और सत्त्व से उत्तरोत्तर होता हुआ विकास है। परंतु जब हम मनुष्यों को देखते हैं तो स्वयं इन तीन गुणों में भी अनंत वैविध्य पाते हैं। न केवल प्रत्येक जीव ही अपने आप में भिन्न है, अपितु स्वयं व्यक्ति के अपने विकासक्रम के विभिन्न चरणों में हम उसके गठन में वैविध्य या भिन्नता पाते हैं। कोई प्रधानतः तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सदा ही एक ही अवस्था में नहीं रहता। उसके अंदर भी हम समय-समय पर बदलाव आते देखते हैं। इसी ओर श्रीअरविन्द यहाँ संकेत कर रहे हैं कि यदि हम विकासक्रम को केवल तमस्, रजस् और सतत्त्व के आरोहण के द्वारा ही समझाएँ तो उससे इस सारे वैविध्य का रहस्य या उसका औचित्य स्पष्ट नहीं होता। सत्त्व, रजस् और तमस् तो सभी के ऊपर समान ही रूप से लागू होते हैं चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या युवा, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, किसी भी पेशे का क्यों न हो। परंतु फिर भी प्रत्येक के अंदर दूसरे से भिन्नता और विशिष्टता का विधान भी गोचर होता है। साधना के पथ पर भी हम देखते हैं कि किसी समान ही धारा के दो साधकों का विकासक्रम भी भिन्न-भिन्न होता है। किसी समान ही गुरु के पास भी किन्हीं दो साधकों के आंतरिक अनुभव, उनका विकासक्रम भिन्न-भिन्न होता है। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में भिन्न है, प्रत्येक अपने आप में विशिष्ट है। हममें से प्रत्येक उस दिव्य शक्ति की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है जो सभी में तत्त्वतः एक ही समान है। इसी कारण जो घटनाक्रम किसी एक के जीवन में घटित होता है, जिन अनुभवों, उतार-चढ़ावों आदि से वह गुजरता है ठीक वैसा ही पूरी सृष्टि में अन्य किसी के साथ नहीं होता। हालाँकि कुछ चीजों में व्यक्ति का दूसरों से साम्य हो सकता है परंतु वास्तव में भिन्नता तो रहती ही है क्योंकि परमात्मा में इतने अनंतविध तत्त्व और अनंतविध आयाम हैं कि उन्हें किसी भी चीज की पुनरावृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी कारण वनस्पति जगत् तक में भी किसी एक ही पेड़ के दो पत्ते भी हम एक समान नहीं पाते। चाहे भेद कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, परंतु रहता अवश्य है।
प्राचीन भारतीय संस्कृति की यह विलक्षणता रही है कि उसे आरंभ से ही इस वैविध्य का भान था। वह जानती थी कि परमात्मा के अनंत गुण हैं, अनंत आयाम हैं और प्रत्येक जीव के अंदर वे अपनी शक्ति की कोई विशिष्ट अभिव्यक्ति करते हैं। और मानव जीवन का लक्ष्य है अपनी उसी असीम चेतना की ओर विकास करना। श्रीअरविन्द के शब्दों में, "भारतीय संस्कृति आत्मा को हमारी सत्ता के सत्य के रूप में मानती है और हमारे जीवन को आत्मा की अभिवृद्धि एवं विकास के रूप में।...इस आत्मा की ओर, इस परमेश्वर की ओर, सार्वभौम सत्ता, सनातन, अनंत की ओर सीमित चेतना का उत्तरोत्तर विकास, एक शब्द में, उसकी साधारण अज्ञ स्वाभाविक सत्ता का उज्ज्वल दिव्य प्रकृति में विकास के द्वारा आध्यात्मिक चेतना में विकास, यह ही भारतीय विचारधारा के लिए जीवन का अर्थ एवं मानव जीवन का लक्ष्य है।" (CWSA 20: 214)
अतः भारतीय संस्कृति की संपूर्ण तन्मयता एक ऐसी व्यापक व्यवस्था तैयार करने पर थी, या यों कहें कि भागवत् प्रेरणा की क्रिया से स्वयं ही एक ऐसी अतिविशाल संरचना तैयार हो गई जिसका लक्ष्य था प्रत्येक जीव को यथाशीघ्र उसके सच्चे लक्ष्य तक ले जाने में यथासंभव सहायता प्रदान करना। भारत की सामाजिक व्यवस्था इसी अवधारणा पर निर्मित थी। उसका दर्शन, धर्म, साहित्य, कला आदि सभी इसी की अभिव्यक्ति करते थे। सारी शासन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली आदि सभी व्यवस्थाएँ इसी एक लक्ष्य की पूर्ति की संसिद्धि का लक्ष्य रखते थे। समूचे राष्ट्र की सारी छोटी-बड़ी चीजें इस एक ही दिशा में गति करती थीं। इस अनन्य भाव से भावित उत्कंठा ने ही सनातन धर्म को जन्म दिया। सनातन धर्म वह सबसे पूर्ण और प्रभावशाली साधन है जो अत्यंत उदात्त आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर व्यष्टि और समष्टि दोनों को ही यथासंभव प्रभावी रूप से अग्रसर करने की चेष्टा करता है। और इस चेष्टा में उसने व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन को पग-पग पर ऐसे रूपकों, बाह्य अनुष्ठानों, आदर्शों, नीति-विधानों आदि से इस प्रकार परिवेष्टित किया कि ये सभी व्यक्ति और समाज को उस परम लक्ष्य के विषय में सतत् सचेतन रखते थे और उस ओर गति करने में सहायता करते थे भले कोई अपने विकास के पड़ाव पर किसी भी सोपान पर क्यों न खड़ा हो। साथ ही मनुष्य की सत्ता के केवल मानसिक, बौद्धिक या नैतिक भागों की तुष्टि को ही नहीं सता के उसके सतही, सुखभोगवादी भमयों की द्वारा संगे भी प्रदान अपितु सभी भागों को किसी उच्चतर विधान के द्वारा संयमित करने की भी व्यवस्था की गई थी। सत्ता के सतही भागों की तुष्टि के लिए व्रत-त्यौहारी, भानुडान, तंत्र आदि की व्यवस्था की गई थी, इसी प्रकार सत्ता के अन्य अनुशा के लिए भिन्न-भिन्न व्यवस्था की गई थी। मनुष्य की प्रकृति के या उसके विकास की अवस्था के गहरे अध्ययन के आधार पर भारतीय संस्कृति ने मनुष्यों को मोटे रूप से तीन गुणों के विभाजन के अतिरिक्त तिहरे चतुष्टय में बाँटा। ये हैं चार पुरुषार्थ - अर्थ, काम, धर्म और मोक्षः चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास; चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इनमें से जो चातुर्वर्ण्य विभाग है वह किसी पेशे पर नहीं अपितु मनुष्य के मनोवैज्ञानिक ढाँचे पर आधारित है। इस आधार पर किसी एक ही बड़े परिवार में भी ये चारों ही वर्ण देखने को मिल सकते हैं। इन चतुष्टयों के विषय में श्रीअरविन्द कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की "...प्रणाली का ढाँचा एक तिहरे चतुष्टय से गठित था। इसका प्रथम चक्र जीवन के चार प्रकार के लक्ष्यों का समन्वय और क्रम था, प्राणिक कामना और सुखोपभोग, वैयक्तिक और सामाजिक हित, नैतिक अधिकार तथा नियम, और आध्यात्मिक मोक्ष। इसका दूसरा चक्र था समाज की चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था जो सावधानी के साथ क्रमबद्ध की गयी थी तथा अपने निर्दिष्ट आर्थिक कर्त्तव्यों से और गंभीरतर सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक अर्थ से संपन्न थी। इसका तीसरा, अत्यंत मौलिक चक्र और, निःसंदेह, इसके सर्वसमावेशी जीवनादर्शों में अद्वितीय आदर्श था – जीवन की आनुक्रमिक अवस्थाओं का चतुर्विध स्तर-विभाग एवं परंपरा, विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और स्वतंत्र समाजातीत मनुष्य। यह ढाँचा, व्यापक और उदात्त जीवन-शिक्षण की ये प्रणालियाँ इस सभ्यता के परवर्ती वैदिक एवं वीरत्वपूर्ण युग में अपनी शुद्ध अवस्था में, कठोरता और उदारता के अपने महान् स्वाभाविक संतुलन के साथ और अपनी उत्कृष्ट प्रभावशालिता में बराबर बनी रही...” (CWSA 20: 217)
इस प्रकार चार-चार के तीन विभागों के परस्पर संयोजन के द्वारा हमें मानव प्रकृति और उसके विकास की अवस्था के चौंसठ मोटे विभाग मिलते हैं। इनमें यदि तीन गुणों के विभाग को और मिला दिया जाए तो इनके संयोजन से एक-सौ बानवे विभाग मिलते हैं जिनमें मानवों को उनकी प्रकृति और उनके विकास की अवस्था के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। हालाँकि इतने व्यापक विभाजनों के बाद भी ये सभी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होते थे जिसे गुरु के मार्गदर्शन का परम् सौभाग्य प्राप्त हो गया हो। गुरु-वाक्य के अतिरिक्त उस पर अन्य किसी प्रकार का कोई शास्त्र या विधान लागू नहीं होता था। परंतु अपने आप में वह अवस्था भी एक बड़ी ही उच्च अवस्था होती है जब व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रतिनिधिस्वरूप सद्गुरु प्राप्त होने की और उनकी छत्रछाया में विकसित होने की महत् अनुकंपा प्राप्त हो। अतः यह एक बड़ी ही विलक्षण और विरली स्थिति है जो अधिकांश के लिए लागू नहीं होती। अधिकांश को विकास के लिए सहायता की आवश्यकता रहती ही है। और इसी के लिए भारतीय संस्कृति ने तिहरे चतुष्टयों का निर्माण किया।
यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिये कि ये सारे ही चक्र एक सामान्य विकास परंपरा का ही निरूपण करते हैं परंतु एक उन्मुक्त आत्मा के लिए ये बाध्यकारी नहीं होते। जिस भी अवस्था में व्यक्ति को आत्मा का आह्वान प्राप्त हो जाता था उसके बाद यह सर्वमान्य था कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर तब आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई विधान या किसी प्रकार का वर्णाश्रम धर्म बाध्यकारी नहीं होता था। तब वह अपने ही भीतरी विधान के अनुसार जीवन यापन करने और विकास करने के लिए मुक्त हो जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का संपूर्ण ढाँचा मानव प्रकृति, उसके विकास की आंतर और बाह्य अवस्था के एक भली प्रकार अध्ययन पर आधारित था। और ऊपर वर्णित ये सारे विभाजन करने के बाद भी हमारे ऋषियों ने सदा ही देश, काल और पात्र के नियम को ही सर्वोपरि रखा। इस सारी अतिशय जटिलता और नमनीयता का यही कारण था कि भारतीय संस्कृति को परमात्मा की अभिव्यक्ति के वैविध्य का गहरा बोध था जिसकी कि गीता में यहाँ चर्चा आई है। अतः गीता इसी पर बल देती है कि इस वैविध्य के अनुसार व्यक्ति का जो विशिष्ट आंतरिक विधान है, जो कि उसका स्वभाव है उसी का पालन करना उसका स्वधर्म है। अतः व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कि अपनी अंतर्निहित प्रकृति, अपने स्वभाव की खोज करे और अपनी सतही प्रकृति के भाव से अपने उस स्वभाव की ओर गति करे। किसी एक ही परिवार में पैदा हुए तीन बच्चों की सतही प्रकृति तो एक समान हो सकती है परंतु संभवतः तीन बच्चीतरी प्रकृति, उनका स्वभाव, सर्वथा भिन्न-भिन्न प्रकार का हो। उनकी हारतीय संस्कृति सर्वप्रथम व्यक्ति के स्वभाव की खोज करने पर ध्यान देती थी। यदि व्यक्ति का स्वभाव ज्ञान-प्राप्ति का हो और उसे कृषि कार्य में या सेवा-कार्य में लगा दिया जाए तो वह अपने आप को सर्वथा अनुपयुक्त पाएगा। वहीं यदि व्यक्ति का स्वभाव सेवा-कार्य करने का हो और उसे इससे भिन्न किसी कार्य में लगा दिया जाए तो वह उस कार्य को कभी भी सही रूप से नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वभाव नियत कर्म पर बल दिया जाता था। और अपने इस अंतर्निहित भाव या अपने स्वभाव से व्यक्ति को 'मद्भाव' अर्थात् भगवान् के भाव में जाना होता था।
गीता ने इस बात पर कुछ बल दिया है, यहाँ तक कि इसे एक बड़ा भारी प्रारंभिक महत्त्व भी दिया है। अपनी शुरुआत में ही उसने कहा है कि क्षत्रिय का स्वभाव, विधान और कर्तव्य ही अर्जुन के कर्म का निज विधान है, उसका 'स्वधर्म' है; इसके आगे उसने प्रभावपूर्ण बल के साथ इस बात का प्रतिपादन किया है कि अपने निज स्वभाव, धर्म एवं कर्तव्य का पालन और अनुसरण अवश्य करना चाहिए, – भले वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो तब भी वह किसी दूसरे की प्रकृति के धर्म को भली प्रकार अनुष्ठान करने से कहीं अधिक श्रेयस्कर है। परधर्म में विजय-लाभ करने की अपेक्षा स्वधर्म में मृत्यु मनुष्य के लिए कहीं अधिक अच्छी है। परधर्म का अनुसरण अंतरात्मा के लिए भयावह है, हम कह सकते हैं कि यह उसके विकास की स्वाभाविक प्रणाली के विरुद्ध होता है, उस पर यांत्रिक रूप में लादी हुई वस्तु होती है और इसलिये आत्मा के सच्चे स्वरूप की ओर हमारे विकास के लिए एक ऐसी वस्तु होता है जो बाहर से आयातित, कृत्रिम तथा विनाशकारी है। जो कुछ सत्ता के अंदर से बाहर आता है वही उचित और स्वास्थ्यकर वस्तु, यथार्थ प्रवृत्ति है, न कि वह जो बाहर से उस पर लादा जाता है अथवा प्राण की जबरदस्तियों या मन की भ्रांति के द्वारा उस पर थोपा जाता है। यह स्वधर्म चार सामान्य प्रकार का होता है जिसे प्राचीन भारत की सामाजिक संस्कृति के 'चातुर्वर्ण्य' व्यवस्था के कर्म में बाह्य रूप से निरूपित किया गया है। गीता कहती है कि यह वर्ण-व्यवस्था एक दिव्य विधान के क्रमानुरूप ही है, "इसकी सृष्टि गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार मैंने ही की थी", – जिसकी सृष्टि आदिकाल से जगत्पति ने ही की थी। दूसरे शब्दों में, सक्रिय प्रकृति की चार भिन्न श्रेणियाँ हैं, अथवा प्रकृतिगत जीव के चार मूल रूप या 'स्वभाव' हैं, और प्रत्येक मनुष्य का कार्य एवं उपयुक्त कर्तव्य उसके विशिष्ट स्वभाव के अनुरूप होता है। अब इसकी अंतिम रूप से, अधिक सटीक और सूक्ष्मतर ब्यौरों के साथ व्याख्या की गयी है। वर्णाश्रम धर्म और पुरुषार्थ के विषय में तो हम पहले ही विशद चर्चा कर चुके हैं। गीता वर्णों के द्वारा जिस मनोवैज्ञानिक अवस्था की बात करती है उसके अनुसार यदि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हमारी संस्कृति में हम वैश्यों की प्रधानता पाते हैं और अन्य वर्णों की न्यूनता पाते हैं।
प्रश्न : जब अपने विशुद्ध रूप में वर्णों को आंतरिक प्रकृति के द्वारा निर्धारित मानते हैं तब फिर क्या आनुवांशिकता के द्वारा भी गुण संतति में हस्तांतरित होते हैं?
उत्तर : यह एक बड़ा ही जटिल विषय है जिसका कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। अवश्य ही आनुवांशिकता से कुछ गुण हस्तांतरित होते हैं और इसी कारण जातिगत विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। परंतु अधिकांशतः जब हम आनुवांशिकता की बातें करते हैं तब उसे व्यापारिक पेशों से समझ बैठते हैं जबकि वर्ण कोई सतही नहीं अपितु आंतरिक विषय है। महाभारत आदि में हम देखते हैं कि कई बार पूरे के पूरे क्षत्रिय वंश ब्राह्मणों के कार्य करने लगते हैं और इसी प्रकार ब्राह्मण वंश क्षत्रियों के कार्य करने लगते हैं। साथ ही जब अंतर्जातीय विवाह आदि होने लगे तब वर्णों का सम्मिश्रण होने लगा इसलिए बाहरी जातियों का ढाँचा तो इससे और अधिक विशुद्ध रूप में नहीं रह पाया परंतु तब भी जो भीतरी प्रकृति है उसके अनुसार व्यक्ति के भिन्न-भिन्न स्वभाव का नियम तो फिर भी लागू होता है। साथ ही, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस वर्ण-व्यवस्था का भारतीय संस्कृति में हम उल्लेख पाते हैं वह केवल आर्यों पर ही लागू होती है। आर्य का अर्थ है वह व्यक्ति जो आत्म-अतिक्रमण करने की, अपनी जिस किसी भी स्थिति में वह है उससे आगे जाने की अभीप्सा करता है और उसके लिए चेष्टा करता है। अतः आर्य संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्तमान स्तर से सदा ही विकसित होकर उच्चतर चेतना में जाने की चेष्टा करता था। इस दृष्टि से ब्राह्मण और शूद्र में कोई भेद नहीं था। एक शूद्र जो सतत् आत्म-अतिक्रमण की चेष्टा करता था वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता था जो अपनी स्थिति से संतुष्ट हो।
जहाँ तक जातिगत विशेषता और आनुवांशिकता की बात है तो उन्नीसवीं शताब्दी तक यह मान्यता रही है कि यूरोपीय श्वेतवर्ण जातियो उन्नीसवर हैं, अफ्रीकी जातियाँ सबसे निचले स्तर पर हैं और बाकी सभी शीतियाँ इनके बीच में आती हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए विज्ञान को जक पूरी की पूरी शाखा को ही विकसित किया गया। यही मान्यता पूरे एक्क में भारी नरसंहार और रक्तपात का कारण बनी जिसका कि विश्व का इतिहास साक्षी है। परंतु आनुवांशिक विज्ञान में हुई आधुनिकतम खोजे हमें वंशाणुओं (Genes) के अध्ययन के आधार पर डेढ़ लाख साल से भी अधिक पीछे तक के इतिहास तक ले जा सकती हैं और 'द रीयल ईव * पुस्तक में हम पाते हैं कि सबसे पहले अफ्रीका से एक समूह ने लगभग ८५,००० वर्षों पूर्व पलायन किया। वही समूह हिन्दुस्तान से होकर संसार के अन्य सभी भागों में फैल गया। हिन्दुस्तान में करीब २० से ३० हजार वर्षों तक रुकने के बाद ही उनमें से कुछ लोग बाहर जाने लगे। इसी कारण आज जब हम विश्व की सारी संस्कृतियों का बारीकी से अध्ययन करें तो हमें सब में भारतीय मूल के दर्शन होंगे। आज विश्व भर में इस खोज को अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि यह खोज आनुवांशिकीय विज्ञान पर आधारित है। इसी आधार पर प्रमाणित होता है कि विश्व भर में किसी समय वैदिक संस्कृति या उसके अंश अवश्य रहे हैं और संसार के सारे धर्म, दर्शन, मत आदि सभी का वही मूल रहा है। भीतर से सभी जातियों में साम्य होने पर भी जो बाहरी रंग-रूप का हमें अंतर दिखाई देता है वह तो केवल भिन्न बाहरी परिवेश और खान-पान के कारण है।
इसी विज्ञान के आधार पर यह भी अब असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि भारत में भी जो आर्य और द्रविड़ जातियों का भेद किया जाता रहा है वह भी निराधार है। आर्यों द्वारा द्रविड़ भारत पर आक्रमण के निराधार सिद्धांत की आड़ में भारत की अखण्डता को तोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है। स्वामी विवेकानन्द ने तो पहले ही इस सिद्धांत का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में खण्डन कर दिया था कि आर्य और द्रविड़ जाति जैसा कोई भेद है ही नहीं और समस्त भारतीय जन एक ही जाति हैं। अभाव विज्ञान की सहायता से इस सिद्धांत की निस्सारता अकाट्य रूप से अगणित हो ही चुकी है और यह सिद्ध हो चुका है कि रंग-रूप, बोली, अपमान सहन आदि की भिन्नताएँ केवल सतही हैं जबकि मूलतः सभी एक ही वंशवृक्ष से निकलते हैं और सभी एक ही हैं। हालांकि यह बात केवल वर्तमान सृष्टि चक्र के संबंध में है जबकि गीता तो अनेकानेक सृष्टि चक्रों की बात करती है। गीता आनुवांशिकता आदि की बातें नहीं करती। गीता को वर्ण-व्यवस्था तो गुणात्मक है जिसका आनुवांशिकता से कोई अधिक संबंध नहीं है। इसीलिए गीता की शिक्षा के अनुसार किसी एक ही परिवार में एक से अधिक वर्ण भी देखने को मिल सकते हैं। किन्हीं एक ही माता-पिता की चार संतानें भी चार भिन्न-भिन्न वर्णों की हो सकती हैं। इस भेद को हमें सदा ही ध्यान में रखना चाहिये।
------------------------
* The Real Eve by Stephen Oppenhmer, 2004, Publisher: Constable & Robinson Ltd.
अब इस बात पर आते हैं कि किस प्रकार व्यवहार में आनुवांशिकता को वर्ण का आधार माना जाने लगा। इसमें अनेकानेक तत्त्व हैं जो सारे विषय को जटिल बना देते हैं। अतः कोई भी सामान्य नियम तय नहीं किया जा सकता। इसमें से कुछ तत्त्वों की तो हम चर्चा कर सकते हैं जिसके कारण आनुवांशिकता या फिर परंपरागत गति के पीछे का रहस्य समझ में आता है। इसका एक तत्त्व तो यह है कि भारतीय संस्कृति में सामाजिक ढाँचे का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि प्रत्येक वर्ण के लिए सुनिर्धारित धर्म बनाए गए थे जो उस वर्ण के सभी लोगों पर यथायोग्य तरीके से बाध्यकारी होते थे। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए बालक को जन्मकाल से ही ऐसी विधिवत् शिक्षा, ऐसे संस्कार, प्रशिक्षण, अभ्यास आदि प्रदान किये जाते थे कि उसे उस वर्ण में विकसित होने का अनुकूलतम वातावरण व अधिकतम सुअवसर प्रदान किया जा सके। इसी प्रकार सभी वर्णों के अपने-अपने सुनिर्धारित धर्म होते थे जो बहुत ही व्यापक भी होते थे और साथ ही ब्यौरेवार तरीके से व्यक्ति को पग-पग पर दिशानिर्देश भी प्रदान करते थे। परंतु इस व्यवस्था को भी निरंकुश रूप से नहीं लागू किया गया था। यदि किसी का आंतरिक स्वभाव बिल्कुल स्पष्ट हो, या किसी को गुरु के सात्रिध्य का परम् सौभाग्य प्राप्त हो, या फिर व्यक्ति की आत्मा की पुकार प्रबल हो तो ऐसे में यह व्यवस्था उसे एक उच्चतर विधान का पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती थी। और चूंकि इस सारी व्यवस्था में ऋषि ही शीर्षस्थ व्यक्ति होता था और उसका निर्णय अंतिम होता था इसलिए इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की कोई संभावना नहीं थी। साथ ही उसे समाज को देश-काल के अनुसार कोई नया धर्म प्रदान करने का भी अधिकार था। अतः सामान्यतः व्यक्ति को उस वर्ण-विशेष के धर्म से इतना परिवेष्टित कर दिया जाता था कि उसमें विकसित होने का उसे अधिक से अधिक वातावरण प्राप्त हो सके।
इसके अतिरिक्त परंपरा के क्रम को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है उसका एक और तरीका हमें भारतीय संस्कृति में गुरु-परंपरा के द्वारा गोचर होता है। यह एक प्रचलित बात है कि गुरु परंपरा में गुरु जब अपनी परंपरा को आगे ले जाने के लिए किसी योग्य शिष्य को उसका भार सौंपते हैं तो वे केवल उसे अधिकार का हस्तांतरण ही नहीं करते अपितु आध्यात्मिक गुणों का भी हस्तांतरण करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि यह सारा कार्यभार-हस्तांतरण एक भीतर से निर्धारित प्रक्रिया होती है इसलिए शिष्य के अंदर आवश्यक आध्यात्मिक गुण व शक्तियों का अवतरण या प्राकट्य भी होता है। इसीलिए कई बार सतही रूप से सामान्य से प्रतीत होते व्यक्ति को भी जब वह कार्यभार सौंपा जाता है तब हम देखते हैं कि उसमें अप्रत्याशित गुणों का और आध्यात्मिक प्रकाश का प्राकट्य हो जाता है। और यह एक बड़ी ही गुह्य और सूक्ष्म प्रक्रिया है जो कि आज भी गुरुओं की परंपरा में हमें देखने को मिल सकती है जिसका कि किसी भौतिक आनुवांशिकता से कोई संबंध नहीं है। श्रीमाताजी ने भी अपनी कृतियों में इस विषय पर प्रकाश डाला है और स्वयं अपने अनुभव को अभिलिखित किया है कि किस प्रकार श्रीअरविन्द की देह त्याग के बाद जिस प्रकाशपूर्ण मन को श्रीअरविन्द ने सिद्ध किया था वह श्रीमाताजी में हस्तांतरित हो गया। और वे कहती हैं कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का उन्हें ठोस रूप से संवेदन प्राप्त हुआ। अतः चेतना का हस्तांतरण संभव है और होता ही है।
इसके अंदर एक तत्त्व और है जिसे कि बहुत लोगों ने अनुभव किया है और वास्तव में तो संसार में अधिकांश महत् कार्य इसी कारण सिद्ध होते हैं। वह यह है कि अपने जीवन काल में जब व्यक्ति अभ्यास के द्वारा अपने किसी अंग को सिद्ध कर लेता है, पूर्ण रूप से सचेतन बना लेता है तो बहुत हद तक उस अंग विशेष का स्वतंत्र सचेतन अस्तित्व बन जाता है जो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी अपनी अभिव्यक्ति के माध्यमों की खोज करता है। श्रीमाताजी इस विषय में एक पियानो-वादक का उदाहरण देती हैं जो कि एक सामान्य संगीतकार था। परंतु श्रीमाताजी ने कहा कि किसी संगीत प्रस्तुति के दौरान सुअवसर पाकर उसमें किसी मेहतान् पियानो-वादक के हाथों की चेतना का अवतरण हो गया और वही जो पहले सामान्य संगीत बजाता था, उसी ने उस अवतरण के कारण एक विलक्षण संगीत प्रकट किया। अतः इस प्रकार की घटनाएँ भी संभव हैं जिसमें केवल कोई सिद्ध भौतिक अंग ही नहीं, अपितु कुछ विशेष गुणों का भी अवतरण हो सकता है। किसी बिल्कुल कायर व्यक्ति में भी किसी समय परम् शौर्य का अवतरण हो सकता है। कला आदि के क्षेत्र में तो हमें इसके अनेक उदाहरण देखने-सुनने को मिलते हैं। और किसी मात्रा में तो सभी के अंदर यह सूक्ष्म प्रक्रिया चलती ही रहती है। बेदों में इन शक्तियों या क्षमताओं को ऋभु आदि शक्तियों की संज्ञा दी गई है। यदि इस प्रकार पूर्व में विकसित की गई इन क्षमताओं को सुरक्षित रूप से आगामी पीढ़ियों तक हस्तांतरित न किया जा सकता तब तो किसी प्रकार का कोई पार्थिव विकास अधिक संभव ही नहीं हो पाता क्योंकि भले कोई व्यक्ति कितना भी विकास क्यों न कर ले या किन्हीं क्षमताओं को कितने भी विशिष्ट रूप से विकसित क्यों न कर ले, तो भी उसकी मृत्यु के साथ ही वे सभी तो नष्ट हो जातीं। परंतु ऐसा नहीं है। पार्थिव अभिव्यक्ति में जो भी कोई विकास कहीं भी साधित किया जाता है, वह प्रकृति द्वारा संरक्षित रखा जाता है। इसी कारण किसी काल में अमुक प्रगति करने में जितना समय लगता है, आगामी पीढ़ी को उस दिशा में प्रगति करने में उतना समय नहीं लगता। और इसी तरह उत्तरोत्तर विकास चलता रहता है। अतः एक सतत् आदान-प्रदान चलता ही रहता है। पर चूंकि हम सूक्ष्म क्रियाओं को देख और अनुभव नहीं कर पाते इसलिए उनके विषय में हम अनभिज्ञ रहते हैं। परंतु जिनमें भी कुछ सूक्ष्म दृष्टि है वे देख पाते हैं कि किस प्रकार इच्छाएँ, कामनाएँ, आवेग आदि अनेकानेक भाव सदा ही तरंगों के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे अंदर अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रियाएँ पैदा करते हैं। और जहाँ वातावरण सकारात्मक होता है वहाँ इन सब आवेगों आदि का बल नष्ट हो जाता है। हमारे पुराणों आदि में हमें वर्णन मिलते हैं कि किस प्रकार ऋषियों के आश्रमों में हिंसक पशु भी अपनी हिंसक प्रकृति छोड़ देते थे और संयमित रूप से व्यवहार करते थे।
अतः जब कालान्तर में 'स्वभाव' की पहचान - जिसे करना कभी भी आसान नहीं था - जन्म के आधार पर की जाने लगी, क्योंकि बदलती परिस्थितियों में ऐसा करना ही सुगम था, तब एक बाहरी मापदण्ड बदमा) के आधार पर 'स्वभाव' का निर्धारण करने से जो त्रुटियाँ आ (जन्नती हैं उनका परिमार्जन उपरोक्त बतलाये गये प्रत्येक वर्ण विशेष के लिए सुनिर्धारित किये गए धर्म व अत्यन्त बुद्धिमानी व दक्षता से स्थापित किये गए (बाह्य, भावात्मक एवं मानसिक) शिक्षण-प्रशिक्षण के ढाँचे व गुणों के आनुवांशिक हस्तांतरण की संभावनाओं द्वारा किया जाता रहा। यद्यपि यह एक बहुत पूर्ण या दोषमुक्त व्यवस्था नहीं हो सकती थी, फिर भी इसने लंबे समय तक व काफी हद तक वर्ण-व्यवस्था में घोर असंगतियों व विकृतियों को प्रकट होने से रोके रखा।
प्रश्न : इस सारे आनुवांशिकता आदि के वर्णन को हम स्वभाव और स्वधर्म के संदर्भ में किस प्रकार समझ सकते हैं?
उत्तर : स्वभाव और स्वधर्म का संबंध तो हमारी आत्मा के विकास के साथ है। जिन सारी शक्तियों आदि की हम चर्चा करते हैं या बाहरी विकास की चर्चा करते हैं वह तो आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार तय करती है। अंतरात्मा स्वयं अपना परिवेश, मन, प्राण तथा शरीर व उनके गुणों, लक्षणों, क्षमताओं आदि सभी का चयन करती है। और यदि अंतरात्मा अभी अधिक विकसित न हो तो ऐसी सहायक सत्ताएँ होती हैं जो उसे इस चयन में सहायता करती हैं। और अभिव्यक्ति में किस प्रकार आगे से आगे विकास होता है उसकी हमने इससे पूर्व चर्चा की है। साथ ही इसमें हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि साधना के द्वारा बाहरी ढाँचे को किसी भी हद तक बदला जा सकता है अन्यथा साधना का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। इसी कारण हम पाते हैं कि साधना के द्वारा ऋषियों के अंदर वे शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती थीं जिनसे भौतिक नियमों में भी वे अपनी इच्छानुसार फेर-बदल कर सकते थे। किसी नेत्रहीन को नेत्र प्रदान करना, किसी रोगी व्यक्ति को निरोग करना आदि जैसी चीजें उनके लिए सहज हो जाती हैं। परंतु जहाँ तक स्वभाव की बात है, व्यक्ति को सच्या दिशानिर्देश तो केवल सद्गुरु के प्राप्त होने पर ही मिल सकता है अन्यथा तो अपने सच्चे स्वभाव के बारे में सचेतन होना बहुत ही मुश्किल है।
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ।। ४०।।
४०. न तो पृथ्वी पर और न ही स्वर्ग में देवों के मध्य कोई भी ऐसा प्राणी है जो प्रकृतिजन्य इन तीन गुणों से मुक्त हो।
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ।। ४१।।
४९. हे परंतप। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्म उनके स्वभावजन्य गुणों के अनुसार विभक्त हुए हैं।
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ।। ४२।।
४२. शांत-स्थिरता, आत्मसंयम, तपस्या, शुचिता, सहनशीलता, सरल व्यवहार अथवा स्पष्टवादिता, ज्ञान तथा विज्ञान (मूलभूत तथा व्यापक ज्ञान), आध्यात्मिक सत्य की स्वीकृति तथा उसका अभ्यास ब्राह्मण के कर्म हैं जो उसके स्वभाव से उत्पन्न होते हैं।
सामान्यतः जब कर्म के विभाजन की बात आती है तब प्रायः ही हम उन्हें बाहरी कर्मों से या पेशे से मान बैठते हैं। जबकि ब्राह्मण के जिन कर्मों का गीता यहाँ वर्णन करती है उनसे तो सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि गीता का कर्म के द्वारा अभिप्राय किसी बाहरी पेशे से नहीं हो सकता अपितु ये सभी तो आंतरिक गुण हैं। 'शांत-स्थिरता, आत्मसंयम, तपस्या, शुचिता, सहनशीलता, सरल व्यवहार अथवा स्पष्टवादिता, ज्ञान तथा विज्ञान (मूलभूत तथा व्यापक ज्ञान), आध्यात्मिक सत्य की स्वीकृति तथा उसका अभ्यास' - इन सब में अभ्यास को तो हम बाहरी कर्म की श्रेणी में डाल सकते हैं परंतु इसके अतिरिक्त आत्म-संयम, शुचिता, सहनशीलता आदि तो कोई कर्म नहीं हो सकते। अब यदि इन मानदंडों से हम ढूँढ़ें तो कदाचित् ही हमें कोई ब्राह्मण मिले। केवल ब्राह्मण ही क्यों, गीता जिस-जिस प्रकार के गुण चारों वर्णों के बताती है उस दृष्टिकोण से तो कदाचित् ही हमें अपने विशुद्ध रूप में कोई भी वर्ण दिखाई दे। क्योंकि वर्ण केवल आर्य व्यवस्था में ही होते थे। यह हम पहले भी कह चुके हैं कि आर्य का अर्थ है वह जो सदा ही अपने आत्म-अतिक्रमण के लिए परिश्रम करता रहता है और जो अपनी जिस किसी भी स्थिति पर, चाहे वह कितनी भी उच्च स्थिति ही क्यों न हो, संतुष्ट होकर ठहर नहीं जाता। इसी आधार पर यदि कोई ब्राह्मण अपनी स्थिति से संतुष्ट होकर ठहर जाता है और आगे जाने की अभीप्सा नहीं करता वह फिर आर्य "कहलाने योग्य नहीं रहता अपितु म्लेच्छ हो जाता है। वहीं कोई शुद्र चाहे कह कितनी भी पतित अवस्था में ही क्यों न हो, या कर्म की दृष्टि से भले वहतना भी तुच्छ कर्म क्यों न करता हो, परंतु यदि उसके अंदर अपने कर्म के प्रति किसी प्रकार की कोई जुगुप्सा नहीं है और उसके द्वारा वर कपना आत्म-अतिक्रमण साधित करने के लिए प्रयास करता है तो यह आर्य है। आगे आने वाले वर्णन में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार गीता प्रत्येक वर्ण के अनुसार जो कर्म बताती है वह कोई बाहरी पेशा नहीं अपितु आंतरिक गुण है। जहाँ बाहरी कर्म का भी कुछ संकेत है वह भी वास्तव में उस आंतरिक वृत्ति पर ही आधारित है।
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
दानमीश्वरभावश्व क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ।। ४३ ।।
४३. शूरवीरता, तेज या साहस-बल, दृढ़ निश्चयता, दक्षता और युद्ध से पलायन न करना, दान और शासन करना क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं।
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ।। ४४।।
४४. कृषि, गोपालन और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं; सेवा स्वभाववाले समस्त कर्म शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं।
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ।। ४५।।
४५. अपने स्वयं के कर्म में निष्ठापूर्वक लगे रहते हुए मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है; अपने कर्म में लगा हुआ कोई किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है, वह तू सुन।
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ।। ४६।।
४६. जिस (परमात्मा) से समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे यह सब (जगत्) व्याप्त है, उसकी अपने कर्म के द्वारा अभ्यर्चना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ।। ४७।।
४७. भली प्रकार अनुष्ठित किये गये किसी परधर्म से, अपने-आप में दोषपूर्ण होते हुए भी, स्वधर्म श्रेड होता है; अपने स्वधान द्वारा नियत ( किये हुए कर्म को करने पर मनुष्य पाप को नहीं प्रास होतात
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ।। ४८।।
४८. हे कौन्तेया सहज (स्वभावजन्य) कर्म को दोषयुक्त होते हुए भी नहीं छोड़ना चाहिये; क्योंकि समस्त कार्यों के आरम्भ दोषों से वैसे ही आच्छादित रहते हैं जैसे धुँए से अग्नि आच्छादित रहती है।
त्रिगुण के क्षेत्र में समस्त कर्म ही अपूर्ण होता है, समस्त मानव-कर्म ही दोष, अशुद्धि या सीमितता से बाध्य होता है; परंतु इस कारण हमें अपने निज विशिष्ट कर्म तथा स्वाभाविक कर्तव्य का परित्याग नहीं कर देना चाहिये। कर्म होना चाहिये समुचित रूप से नियमित कर्म, 'नियतं कर्म', परंतु आंतरिक अथवा मूलभूत रूप से अपना निज कर्म, अपने अंदर से विकसित, अपनी सत्ता के सत्य के साथ समस्वर, स्वभाव के द्वारा नियत, 'स्वभावनियतं कर्म'।
यहाँ गीता का ठीक-ठीक अभिप्राय क्या है? पहले हम इसे इसके बाह्यतर अर्थ में देखें और इस पर विचार करें कि गीता ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे जाति और युग के विचारों ने क्या पुट दिया था - उस पर सांस्कृतिक परिवेश का क्या रंग चढ़ा हुआ है और उसका प्राचीन अर्थ क्या है। ये श्लोक तथा इसी विषय पर गीता ने पहले जो वचन कहे हैं वे जाति-भेद-विषयक आधुनिक शास्त्रार्थों में प्रमाणरूप से उद्धृत किये जाते रहे हैं और कुछ लोगों द्वारा इसकी व्याख्या इस रूप में की गई है कि ये वर्तमान प्रथा का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरों के द्वारा इनका प्रयोग जाति-भेद के आनुवांशिक आधार का खंडन करने के लिए किया गया है। पर वास्तव में गीता के श्लोकों का प्रचलित जाति-भेद के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह चतुर्वर्ण के, अर्थात् आर्यजाति के चार सुस्पष्ट वर्गों के प्राचीन सामाजिक आदर्श से अत्यंत भिन्न वस्तु है, और यह गीता के वर्णन के साथ किसी प्रकार भी मेल नहीं खाता। कृषि, गोपालन और प्रत्येक प्रकार के व्यापार को यहाँ वैश्य के कर्म बताया गया है; किंतु बाद की जाति-व्यवस्था में उन लोगों में से, जो व्यापार तथा पशु-पालन का कार्य करते थे, बहुतों को, शिल्पियों तथा छोटे-मोटे कारीगरों एवं अन्य कई को वास्तव में शूद्र-वर्ग में सम्मिलित किया गया है, - वह भी वहाँ जहाँ उन्हें चतुर्वर्ण के घेरे से बिल्कुल बाहर ही नहीं कर दिया गया है, - और कुछ एक अपवादों को छोड़कर केवल वणिक-वर्ग को ही वैश्य की श्रेणी में रखा गया है, और वह भी सर्वत्र नहीं। कृषि, शासन कर और सेवा तो आज ब्राह्मण से लेकर शुद्र पर्यंत सभी वर्णों के पेशे हैं। और जहाँ कर्तव्य कर्म के आर्थिक विभागों में इतना अधिक घोटाला कर दिया गया है कि उनमें सुधार की कोई संभावना ही नहीं दीखती, वहाँ गुण के अनुसार कर्म का विधान परवर्ती जाति-भेद-प्रथा में और भी कम स्थान रखता है। उसमें तो सब कुछ एक कठोर आचार ही है जिसका वैयक्तिक प्रकृति की आवश्यकता से कुछ भी संबंध नहीं। उधर यदि हम इस विवाद के उस धार्मिक पहलू को लें जिसे जाति-भेद के समर्थकों ने प्रस्थापित किया है तो हम, निश्चय ही, गीता के शब्दों के साथ ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण विचार नहीं जोड़ सकते कि मनुष्य की प्रकृति का धर्म यह है कि वह अपनी वैयक्तिक प्रवृत्ति एवं क्षमताओं का विचार किये बिना अपने माता-पिता या निकट या सुदूर पूर्वजों के पेशे को ही अपनाये, ग्वाले का पुत्र ग्वाला ही बने और डाक्टर का पुत्र डाक्टर, मोची की संतति कालचक्र के आवर्तन-पर्यंत मोची ही बनी रहे: फिर इस विचार को तो गीता पर और भी कम थोपा जा सकता है कि ऐसा करने से, व्यक्तिगत पुकार एवं व्यक्तिगत गुणों का विचार किये बिना दूसरे की प्रकृति के धर्म को इस प्रकार विवेक-रहित होकर यंत्रवत् दोहराते रहने से मनुष्य अपनी पूर्णता की ओर सहज ही अग्रसर होता है तथा आध्यात्मिक स्वातंत्र्य प्राप्त करता है। गीता के शब्द तो चतुर्वर्ण की प्राचीन व्यवस्था के उस रूप की ओर संकेत करते हैं जो अपनी आदर्श शुद्धावस्था में विद्यमान था या विद्यमान समझा जाता था, कई लोगों का कथन है (और यह कथन कुछ विवादग्रस्त है) कि यह व्यवस्था एक आदर्श या एक साधारण नियम के अतिरिक्त और कुछ कभी भी नहीं रही तथा व्यवहार में इसका अनुसरण न्यूनाधिक शिथिलता के साथ ही किया जाता था, हमें उसी प्रचलित व्यवस्था को दृष्टि में रखकर इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ भी, इसका सटीक बाह्य अर्थ समझने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव होती है।
जब हम आंतरिक अर्थ चूक जाते हैं तभी चतुर्वर्ण की व्यवस्था को जातिवाद समझ बैठने की भूल कर बैठते हैं। और फिर इसके आधार पर जातिगत अभिमान रखना और यह समझना कि गीता जातिगत श्रेष्ठता के अभिमान का समर्थन करती है और इसी जातिगत श्रेष्ठता के द्वारा व्यक्ति को भागवत् प्राप्ति हो सकती है, ये सभी बिल्कुल निराधार बातें हैं। वर्ण तो सर्वथा आंतरिक और मनोवैज्ञानिक विषय है। केवल आंतरिक सत्ता ही निश्चित कर सकती है कि व्यक्ति की प्रकृति क्या होगी और उसके बाहरी कर्म क्या होंगे। उदाहरण के लिए ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेने से यह निर्धारित नहीं हो जाता कि व्यक्ति में ब्राह्मण के जो गुण बताए गए हैं वे आ जाएँ। वहीं सत्यकाम जाबाल जैसे किसी उदाहरण में संभव है कि व्यक्ति को अपने गोत्र तक का भी पता न हो और फिर भी उसमें ब्राह्मणत्व के गुण हों। अतः वर्ण व्यवस्था से गीता का अभिप्राय प्राचीन वर्ण व्यवस्था से है जो गुणों पर आधारित है और जिसका वर्तमान जातिप्रथा से कोई संबंध नहीं है। साथ ही प्रत्येक वर्ण के कर्मों के विषय में गीता का जो वर्णन है उससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में ये सभी कर्म आंतरिक हैं।
गीता के वर्णन को यदि बाहरी रूप से भी लिया जाए तो गीता गोपालकों, शिल्पियों और कारीगरों को वैश्य श्रेणी में रखती है जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन्हें शूद्र श्रेणी में रखा जाता है। हालाँकि वास्तव में तो वैश्य बाहरी कर्म से नहीं अपितु आंतरिक गुण से निर्धारित होता है। आर्य पद्धति के अनुसार वैश्य में कार्यकुशलता, चीजों के बीच परस्पर संबंध का बोध, कार्य को करने के उचित विधान आदि का बोध होता है। वह विभिन्न चीजों के बीच परस्पर संबंध को जानकर उनमें सामंजस्य स्थापित कर सकता है। वहीं शूद्र में सेवा का अंतर्निहित भाव होता है। यद्यपि प्राचीन वर्ण व्यवस्था में शूद्र को हीन नहीं माना जाता था, परंतु कालांतर में जब वर्ण व्यवस्था को जाति प्रथा मान लिया गया तब शूद्र को सबसे निचले दर्जे का माना जाने लगा जबकि यदि यह गुण न हो तो इसके अभाव में अन्य सभी वर्णों की क्रियाएँ संपादित ही नहीं हो सकतीं। इसी प्रकार चारों में से यदि कोई एक गुण भी न हो तो उसके अभाव में पूर्ण क्रिया साधित नहीं हो सकती। किसी कर्म को पूर्ण रूप से संपादित होने के लिए चारों ही गुणों की समन्वित क्रिया आवश्यक है। हालाँकि सभी में कुछ न कुछ मात्रा में चारों ही वृत्तियाँ होती हैं परंतु जब इन सभी का पूर्ण रूप से विकास होता है तब व्यक्ति भगवान् के मद्भाव की ओर जा सकता है। अतः गीता की शिक्षा यही है कि व्यक्ति के अंदर जिस भी शक्ति की या स्वभाव की प्रधानता हो उसी के अनुसार वह आरंभ करे। और ज्यों-ज्यों व्यक्ति विकसित होता जाता है त्यों-ही-त्यों स्वभाव के अन्य पक्षों का एवं अन्य शक्तियों का भी विकास होता जाता है। यदि किसी को सद्गुरु प्राप्त हो जाएँ तो उसके बाद फिर उसे किसी भी वर्ण या आश्रम आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती और तब गुरु-वाक्य ही उसका परम् विधान होता है और वे ही व्यक्ति को यथाशीघ्र उसके सच्चे गंतव्य तक ले जाते हैं।
प्राचीन वर्ण-व्यवस्था जब अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं रही तब भी उसका कुछ-न-कुछ अंश अवश्य बना रहा और प्रत्येक वर्ण अपने शास्त्रसम्मत कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करने का प्रयास करता था। इस वर्ण-व्यवस्था के अपभ्रष्ट रूप जाति-प्रथा - में भी जो भयंकर विकार आए उनमें मुस्लिम और अंग्रेजी आक्रांताओं के शासन ही प्रधान कारण रहे। इन्हीं शासन कालों के दौरान भारत के उज्ज्वल इतिहास को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया गया और जातियों के विषय में ऐसा चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया कि ब्राह्मण अन्य जातियों के साथ अपनी श्रेष्ठता के अभिमान में निरंकुश व्यवहार करते थे, क्षत्रिय अपने बल के आधार पर जनता पर अत्याचार करते थे, वैश्य अपने व्यापार आदि में दूसरों के साथ पारदर्शी व्यवहार नहीं करते थे, और शूद्र सभी जातियों के द्वारा पददलित थे जिन्हें किसी प्रकार की शिक्षा, सम्मान आदि का कोई अधिकार नहीं था। परंतु श्रीअरविन्द और स्वामी विवेकानन्द ऐसी सभी बातों को बिल्कुल निराधार बताते हैं और भारतीय इतिहास का एक बहुत ही उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत करते हैं। जो तथ्य वे सामने लाते हैं उन्हें जानकर किसी भी व्यक्ति में सहज ही भारतीय अतीत पर गौरव और गहरी श्रद्धा का भाव जागृत हो जाएगा। और इतिहास के विषय में अधिकाधिक अनुसंधान करने पर हम न केवल उनके कथनों को बिल्कुल सटीक पाते हैं अपितु साथ ही हमें यह आश्चर्य भी होता है कि सभी प्रचलित भ्रांतियों के चलते भी उनकी भारतीय संस्कृति और उसके अतीत के विषय में कैसी गहरी समझ और पैनी दृष्टि रही होगी जो प्रतीतियों के पीछे भी देख सकती थी। परंतु दुर्भाग्यवश आज सूचना की विकसित तकनीकें होने के बाद भी भारतीय जन, और विशेषकर पाश्चात्य प्रभाव में पूरी तरह रंगा युवा वर्ग, भारतीय संस्कृति की इस महानता के विषय में सर्वथा अनभिज्ञ है और इसी कारण अपनी संस्कृति के प्रति किसी प्रकार का गौरव अनुभव करने की बजाय वह इसे अवमानना दृष्टि से देखता है और पश्चिम की ओर आशा जमाए बैठा है।
आज जब हम भारत के इतिहास को, जो कि हमारे आक्रांताओं द्वारा न लिखा गया हो, पढ़ते हैं तो पाते हैं कि भारत सदा ही परम् वैभवशाली और संपन्न राष्ट्र रहा है। दरिद्रता कभी भी भारतीय लक्षणों में नहीं रही। जितने भी विदेशी आक्रांता यहाँ आए वे केवल व्यापार और मार्थिक लाभ की दृष्टि से यहाँ आए थे। यह तो एक जाहिर सी बात है कि यदि जैसी दरिद्रता का चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है यदि वह सच होता तो यह एक बिल्कुल बेतुकी बात होती कि सुदूर देशों से बे आक्रांता यहाँ आते? आज हमें रमेश चन्द्र दत्त जैसे अनेकों इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ही इंग्लैंड भेजे पत्रों आदि के माध्यम से तथा अन्य सूत्रों से यह पता लगता है कि किस प्रकार योजनाबद्ध रूप से भारत को सारी संपदा को लूटा गया। यही नहीं, दीर्घ काल तक लगातार एक के बाद एक और एक से एक भीषण मानवनिर्मित दुर्भिक्ष पैदा किये जिनमें करोड़ों लोग भूख से मर गए और पूरे राष्ट्र की व्यवस्था चरमरा गई। विदेशियों के सारे प्रयास के पीछे निहित उद्देश्य था कि पूरी संस्कृति की कमर तोड़ दी जाए और उसे नष्ट कर दिया जाए।
हमारी संस्कृति के मूल स्तंभ, वेदों, को भी सर्वथा अवमानित करने का प्रयास किया गया। दुर्भाग्यवश आज भी हम मैक्स म्यूलर को वेदों के पंडित और भारतीय संस्कृति के परम् हितैषी के रूप में मानकर उसके द्वारा लिखी पुस्तकों का अध्ययन-अध्यापन करते हैं जबकि आज उसके वे पत्र प्रकाश में आ चुके हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि स्वयं मिशनरी न होते हुए भी उसका कार्य मिशनरी भाव से प्रेरित था। यहाँ हम के. वी. पालीवाल की पुस्तक Max Muller: A Secular Christian Missionary and Distorter of the Veda, Hindu Writers Forum, New Delhi, 2006 के कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं जिनसे हमें यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वेदों को नष्ट करने की कुत्सित योजना किस हद तक चल रही थी।
१८६८ में उसने आर्गाइल के राजकुमार, जो कि भारत के तात्कालिक राज्य-सचिव (Secretary of State) थे, को लिखा, "मिशनरियों ने इतना काम कर डाला है जितना कि वे स्वयं भी उसके बारे में अभिज्ञ नहीं होंगे, यही नहीं, जो उनका बहुत-सा काम है उसे तो वे स्वीकार ही नहीं करेंगे कि वह उन्होंने किया है। हमारी १९वीं शताब्दी की ईसाइयत शायद ही भारत की ईसाइयत हो पाएगी। किंतु भारत का पुरातन धर्म तो अभिशप्त है - और यदि इसमें ईसाइयत वहाँ प्रवेश नहीं करती तो इसमें दोष किसका होगा?" (पृष्ठ २७)
मैक्स मूलर का वेदों का अनुवाद भारी रूप से निहित हेतुओं से प्रायोजित था परंतु अपने अंतरंग निजी पत्रों के अलावा उसने ऐसा खुल तौर पर कभी भी प्रकट नहीं किया। ऐसा ही एक पत्र उसने अपनी परी को दिसंबर १८६६ में लिखा, "मुझे आशा है कि मैं अपना वह काम पूरा कर लूंगा और हालाँकि यह देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूँगा, पर फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरा यह संस्करण तथा वेद का अनुवाद आने वाले समय में भारत के भाग्य पर बहुत हद तक प्रभाव डालेगा और उस देश के लोगों के विकास को प्रभावित करेगा। यह उनके धर्म का मूल है, और उन्हें यह दिखाना कि वह मूल क्या है, मुझे लगता है, यही उस सबका उन्मूलन करने का एकमात्र तरीका है जो कुछ पिछले तीन हजार वर्षों के दौरान उसमें से पैदा हुआ है।" (पृष्ठ २६)
इस पत्र से १० वर्षों पूर्व मैक्स मूलर द्वारा लिखे एक दूसरे पत्र से उसके क्रिश्चियन मिशनरी हेतुओं के विषय में कोई संशय शेष नहीं रह जाता। २५.८.१८५६ को मि. बन्सन को वह लिखता है, "... अंतिम कब्जे के बाद भारत के इलाकों को विजय करने का काम समाप्त हुआ - अब इसके बाद धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में संघर्ष होगा जिसमें निश्चय ही राष्ट्रों की दिलचस्पी लगी हुई है। ईसाइयत के लिए भारत इतना तैयार है जितने रोम या ग्रीस भी सेंट पॉल के समय भी तैयार नहीं थे। उस सड़े हुए बेकार पेड़ को कुछ बाहरी सहारों से रोके रखा था क्योंकि उसका गिरना (ब्रिटिश) सरकार के लिए असुविधाजनक होता। परंतु यदि अंग्रेजी समुदाय को लगता है कि देर-सवेर उस पेड़ को अवश्य गिरना ही है तो फिर ऐसा तय है। वह फिर किसी भी प्रकार के बलिदान से नहीं चूकेगा चाहे वह रक्त का हो या भूमि का। इस संघर्ष के हेतु मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। दलीप सिंह बहुत कुछ हमारे समर्थन में हैं और निश्चय ही भारत में वह एक राजनैतिक भूमिका निभाएँगे। मेरी इच्छा थी कि बिल्कुल सामान्य रूप से उनसे संपर्क साध पाता। क्या कोई ऐसा प्रबंध प्रिंस अल्वर्ट की सहायता से हो सकता है या इसमें तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? मैं भारत में एक मिशनरी के रूप में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता , इससे व्यक्ति पादरियों-पुरोहितों का मोहताज हो जाता है, कोई जन सेवक (Civil servant) के तौर पर जाना चाहता, क्योंकि उससे मैं सरकार पर आश्रित हो जाता हूँ। मैं वहाँ दस साल काफी शांति के साथ रहकर भाषा सीखना चाहता हूँ, संगी-साथी बनाना चाहता हैं और तब मैं देखूंगा कि मैं उस कार्य में भाग लेने हेतु उपयुक्त था या ही जिस कार्य से भारतीय पुरोहित वर्ग की पुरानी बदमाशी को उठाकर भरका जा सके तथा सरल ईसाई शिक्षा के प्रवेश का मार्ग खोला जा सके, ऐसा प्रवेश जो यह शिक्षा प्रत्येक मानव हृदय में पाती है, जो पुरोहितों की जालसाजी की सामर्थ्य से तथा दार्शनिकों के मतिभ्रम पैदा करने वाले प्रभाव से मुक्त हो। जो कुछ भी भारत-मूल में पैदा होता है वह शीघ्र ही पूरे एशिया में छा जाता है, अतः ईसाइयत की प्राण शक्ति अपने आप को अन्यत्र कहीं इतने भव्य रूप से चरितार्थ नहीं कर पाएगी जितना कि वहाँ (भारत में) जहाँ संसार उसे पुनः एक बार उदय होते देखेगा, हालाँकि पश्चिम में इसका जो रूप है उससे बिल्कुल भिन्न रूप में, किन्तु फिर भी अपने सार रूप में यह वैसी ही होगी।" (पृष्ठ २०-२१)
इसी प्रकार भारतीय शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल योजनाबद्ध रूप से नष्ट-भ्रष्ट किया गया। १८५७ के विद्रोह से पहले, ब्रिटिश अधिकारियों ने सक्रिय रूप से ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण की क्रियाओं को बढ़ावा दिया। इस रणनीति के पीछे न केवल धार्मिक कट्टरपंथी अपितु उपनिवेशकारी निहित स्वार्थ शामिल थे। इस संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था टी. बी. मैकॉले (१८००-१८५९) - एक शिक्षाविदजो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने में और उस शिक्षा के साथ ही भारतीय शिक्षा पद्धति में यूरोपीय ईसाइयत के प्रति वरीयता का पक्षपात लाने में माध्यम बना। १९४७ में मिली स्वतंत्रता के बाद भी वही शिक्षा न केवल ज्यों की त्यों जारी रही है बल्कि पिछले दो दशकों में पूर्ण रूप से हावी हो गई है। मैकॉले की आशा थी कि उच्च सुसंस्कृत वर्गीय भारतीयों के बीच अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार ईसाइयत के प्रचार-प्रसार में और उसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश राज का शासन स्थापित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते उसने अंग्रेजी स्कूलों का एक नेटवर्क तैयार करने का काम किया। भारतीयों द्वारा इन स्कूलों की बड़े ही उमंग के साथ स्वीकृति ने भारत में ईसाइयत की भावी संभावनाओं को लेकर उसकी आशाओं को बड़े भारी रूप से बढ़ा दिया। १८३६ में अपने पिता को लिखे एक पत्र में वह कहता है, "हमारी अंग्रेजी स्कूलें बड़े आश्चर्यजनक रूप से फल-फूल रही हैं। सभी इच्छुक लोगों को हम शिक्षण प्रदान करने में मुश्किल अनुभव कर रहे हैं - और वास्तव में कुछ स्थानों पर तो शिक्षण संभव ही नहीं है। अकेले हुगली नगर में १४०० लड़के अंग्रेजी सीख रहे हैं। हिन्दुओं पर इस शिक्षा का प्रभाव अनिष्टकारक हुई कोई भी हिन्दू जिसने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर ली है वह कभी भी सच्चाई के साथ अपने धर्म से जुड़ा नहीं रहता। कुछ उसे (हिन्दू धर्म को) एक नीति के रूप में अपनाए रहते हैं; बहुत से अपने आप को शुद्ध देवतावादी बताते हैं और कुछ ईसाइयत अपना लेते हैं। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजनाओं का अनुसरण जारी रहा तो ३० साल बाद बंगाल के संभ्रांत वर्ग में एक भी मूर्तिपूजक नहीं बचेगा। और यह सब धर्मांतरण कराने के किन्हीं प्रयासों के बिना ही सिद्ध हो जाएगा; वह भी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ जरा भी हस्तक्षेप किए बिना, मात्र ज्ञान व चिंतन की स्वाभाविक क्रिया द्वारा। मैं हार्दिक रूप से इन भावी संभावनाओं से आनंदित होता हूँ ...." (पृष्ठ १५)
ये सभी तथ्य पढ़कर कोई भी अवाक् रह जाएगा कि किस प्रकार इस राष्ट्र को उसके प्रत्येक अंग में पूर्णतः नष्ट करने का सुनियोजित प्रयास किया गया और दुर्भाग्यवश आज भी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित भारतीयों का एक बड़ा भाग अपने ही मूल को हीन दृष्टि से देखता है। परंतु इतना सब होने के बाद भी भारतीय आत्मा यथावत् बनी हुई है और आज भारतीय आध्यात्मिकता पूरे विश्व में अधिकाधिक अपना प्रभाव फैलाती जा रही है।
प्राचीन चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था का त्रिविध पहलू था, इसने सामाजिक एवं आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण किया। अपने आर्थिक पहलू की दृष्टि से इसने समुदाय के अंदर सामाजिक मनुष्य के चार कर्तव्य स्वीकार किये, धार्मिक एवं बौद्धिक, राजनीतिक, आर्थिक और सेवासंबंधी कार्य। इस तरह चार प्रकार के कर्म हैं, धार्मिक पौरोहित्य, साहित्य, शिक्षा और ज्ञान का कर्म; शासन, राजनीति, प्रशासन और युद्ध का कर्म; उत्पादन, धनोपार्जन और विनिमय का कर्म; वैतनिक श्रम और सेवा का कर्म। चार सुस्पष्ट वर्गों के बीच इन चार कार्यों के विभाजन के ऊपर समाज की संपूर्ण व्यवस्था को प्रतिष्ठित और सुस्थिर करने का यत्न किया गया। यह व्यवस्था भारत की कोई निराली विशेषता नहीं थी, अपितु किन्हीं भेदों के साथ यह अन्य प्राचीन या मध्ययुगीन समाजों में भी सामाजिक विकास की एक अवस्था का प्रधान लक्षण थी। ये चार कर्म सभी सामान्य समाजों के जीवन में अब भी मूलभूत रूप से अंतर्निहित हैं, परंतु वे स्पष्ट विभाग अब कहीं नहीं है। पुरानी व्यवस्था सर्वत्र भंग हो गयी और उसके स्थान पर एक अधिक अस्थिर व्यवस्था या, जैसा कि हम भारत में देखते हैं, एक अस्त-व्यस्त एवं जटिल सामाजिक रूढ़ता एवं आर्थिक गतिहीनता का जन्म हुआ जो हास को प्राप्त होकर जातियों के संकर में परिणत हो गयी। इस आर्थिक कर्म-विभाग के साथ एक सांस्कृतिक विचार भी जुड़ा हुआ था जो प्रत्येक श्रेणी को उसका धार्मिक आचार, उसका मान-मर्यादा का नियम, नैतिक विधान, उपयुक्त शिक्षा और प्रशिक्षण, चारित्रिक विशेषता, परिवारगत आदर्श एवं अनुशासन- मर्यादा प्रदान करता था। जीवन के तथ्य सदा इस विचार के अनुरूप ही नहीं होते थे, - मानसिक आदर्श और प्राणिक एवं भौतिक व्यवहार के बीच एक प्रकार की खाई सदा ही देखने में आती है, परंतु यथासंभव एक वास्तविक संगति या अनुरूपता बनाये रखने के लिए अनवरत और कठोर प्रयत्न किया जाता था। इस प्रयत्न का महत्त्व, और भूतकाल में सामाजिक मनुष्य के प्रशिक्षण के लिए इसने जिस सांस्कृतिक आदर्श एवं वातावरण की सृष्टि की उसका महत्त्व जितना बखान किया जाए, थोड़ा है; परंतु आज एक ऐतिहासिक, भूतकालिक एवं विकासात्मक अर्थ से अधिक इसका कुछ महत्त्व नहीं। अंतिम बात यह है कि जहाँ कहीं यह वर्णप्रथा विद्यमान थी, वहाँ इसे कम या अधिक, एक धार्मिक समर्थन प्राप्त था (पूर्व में अधिक और यूरोप में बहुत कम) और भारत में तो इसकी एक गंभीरतर आध्यात्मिक उपयोगिता एवं महत्ता भी स्वीकार की जाती थी। यह आध्यात्मिक अर्थ ही गीता की शिक्षा का वास्तविक सार-मर्म है। जब मानव-चेतना में पतन आता है तब व्यक्ति में यह क्षमता नहीं रहती कि वह आंतरिक विधान के अनुसार कर्मों को कर सके और इसलिए उसे बाहरी मानकों या आधारों की आवश्यकता होती है। इसीलिए मानव-चेतना में आई गिरावट के कारण जब वर्ण-व्यवस्था अपना विशुद्ध रूप न रख सकी तो आनुवांशिकता को ही सिद्धान्त मानने की आवश्यकता हुई, क्योंकि आंतरिक मानक के अभाव में समाज की व्यवस्था के लिए किसी बाहरी मानक का होना आवश्यक था। परंतु जिसे हम चेतना का पतन या हास कहते हैं उसका भी अपना गुह्य कारण था। अतः भारतीय संस्कृति में आए इन विभिन्न कालों के अपने गहरे कारण थे। इसका एक कारण था बदलता युगचक्र। इसके विषय में श्रीअरविन्द कहते हैं कि, "हिंदुओं की युगगणना के सिद्धान्त के अनुसार द्वापरयुग में हर चीज नियमबद्ध, विधिबद्ध, विधानबद्ध हो जाती है।
---------------
* निःसंदेह आरंभ में मनुष्य का सामाजिक कार्य और पद परिस्थिति, अवसर, जन्म और सामर्थ्य के द्वारा ही निर्धारित होते थे धाजिक और पद अपेक्षाकृत अव्यवस्थित समाजों में आज भी देखने में आता है; परंतु क्योंकि अतिचार त एक अधिक स्थिर निर्धारित आरंभ हो गया, व्यवहार में उसकी पद-मर्यादा मुख्यतः यो केवल जन्म के द्वारा निर्धारित होने लगी और परवर्ती जाति-प्रथा में जन्म ही पद-मर्यादा का एकमात्र नियामक बन गया।
... यह एक अनिवार्य विकास था, क्योंकि बाह्य चिह्न ही एकमात्र ऐसे होते हैं जिनका निर्णय सहज रूप से तथा सुविधापूर्वक किया जा सकता है और एक अधिकाधिक यंत्रीभूत, जटिल और लोकाचारात्मक समाज-व्यवस्था में जन्म ही वर्ण-निर्धारण का एक अत्यंत सहज और सुविधाजनक लक्षण था। वंश-परंपरानुगत कार्य में तथा व्यक्ति के वास्तविक अंतर्भूत स्वभाव और सामर्थ्य में जो विरोध-वैषम्य हो सकता था उसे कुछ काल तक तो शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा दूर या कम किया जाता रहा, किंतु अंत में इस प्रयत्न को स्थिर रूप से जारी नहीं रखा जा सका और वंशानुगत प्रथा को ही चरम नियम मान लिया गया।
सत्ययुग में भगवान् विष्णु 'यज्ञरूप' धारण करके मनुष्यों में अवतरित होते हैं। 'यज्ञ' श्रद्धा-भक्ति तथा आत्मनिवेदन का भाव है, तथा सत्ययुग में मनुष्यों के हृदयों में यज्ञ का साम्राज्य होता है, तथा बाहरी विधि-विधान (कर्मकाण्ड), बाहरी यज्ञ-यागादि, सुविस्तृत नियम-कानून, शासन प्रणाली, जातिभेद, वर्गभेद, धार्मिक मत-मतान्तरों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। मनुष्य अपनी परिशुद्ध प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार तथा अपने सम्पूर्ण ज्ञान के आधार पर धर्म (नियम) का पालन करते हैं। ईश्वर का साम्राज्य तथा वेदों का 'उसकी' (ईश्वर की) प्रजा के हृदय में निवास होता है। त्रेतायुग में प्राचीन सम्यक् व्यवस्था टूटनी शुरू हो जाती है तथा भगवान् विष्णु 'चक्रवर्ती राजा' के रूप में, योद्धा तथा शासक के रूप में, अवतरित होते हैं, यथा कार्तवीर्य, परशुराम तथा राम, और शस्त्र तथा शास्त्र, एवं लिखित वेद, मनुष्यों पर शासन करने के लिए संस्थापित किये जाते हैं। किंतु अभी भी अत्यधिक मात्रा में नमनीयता तथा स्वतंत्रता बनी रहती है तथा एक सीमा के अन्दर मनुष्य अपनी उस प्रकृति की स्वस्थ प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं, जो अपनी पवित्रता से प्रथम अवनति के कारण थोड़ा सा भ्रष्ट हो गयी है। द्वापर में आकर चेतना तथा विचारों के स्थान पर उनके बाह्य रूप तथा नियम अब धर्म, नैतिकता तथा समाज के शासक बन जाते हैं। तब भगवान् विष्णु 'व्यास' का रूप धारण करके अवतार लेते हैं; जो ज्ञान को संहिताबद्ध करने वाला तथा पद्धतिबद्ध करने वाला है।
द्वापर के अंत में, जब श्रीकृष्ण आए, तब यह मनोवृत्ति अपने चरम विकास तक पहुँच चुकी थी, तथा केवल बाहरी व्यवहार में ही नहीं अपितु लोगों के दिलों में भी विचार का स्थान बाहरी रूप लेने लगा था और आंतरिक भाव का स्थान नियम लेने लगा था। बहरहाल एक विपरीत वृत्ति भी आरम्भ हो चुकी थी। स्वयं धृतराष्ट्र चीजों के आंतरिक अर्थ को जानने के सच्चे जिज्ञासु थे। महान् वेदान्ती उस समय जीवित थे तथा शिक्षा दे रहे थे, जैसे ऋषि घोर, जिनके समीप स्वयं श्रीकृष्ण ज्ञान प्राप्त करने गए थे। श्रीकृष्ण वह बौद्धिक शक्ति थे जिन्होंने इन सभी बिखरी हुई प्रवृत्तियों को लिया और द्वापर की प्रबल बाह्याचार-निष्ठता को तोड़कर 'कलि' के कार्य के क्षेत्र को तैयार किया। गीता में वे उन लोगों की निंदा करते हैं जो वेद के बाहरी अर्थ की चारदीवारी से बाहर नहीं जाते और (साथ ही) वे यज्ञीय प्रणाली के संपूर्ण सिद्धांत को दार्शनिक अर्थ प्रदान करते हैं, वे रूढ़ नैतिक व्यवस्थाओं के निर्देशन को अवज्ञापूर्वक अस्वीकार कर देते हैं और आचार-व्यवहार के एक आंतरिक और आध्यात्मिक विधान को प्रतिष्ठित करते हैं। प्रतीत होता है कि अपने समय के बहुत से लोगों को वे एक विनाशक और संहारक अपशकुन के समान प्रतीत हुए थे; सभी महान् क्रान्तिकारी प्रवर्तकों की तरह उन्हें भी भूरिश्रवा के द्वारा यह कहकर अवमानित किया गया कि वे लोगों को भटकाने वाले तथा नैतिक मूल्यों को भ्रष्ट करने वाले हैं। यह कलियुग का कार्य है कि वह सभी कुछ पर प्रश्न उठाकर सभी कुछ को नष्ट कर देता है ताकि पवित्रता और अपवित्रता की शक्तियों के बीच संघर्ष के पश्चात् नए सत्ययुग में जीवन के एक नवीन सामंजस्य और ज्ञान को स्थापना कर सके।" (CWSA 18, 263-64)
इस प्रकार इस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि क्यों अपनी शुद्धावस्था में वर्ण आंतरिक गुण थे और किसी प्रकार कोई बाहरी नियम बाध्यकारी नहीं थे। परंतु ज्यों-ज्यों युगचक्र के साथ-साथ चेतना उन्मुक्त न रहकर अधिकाधिक बाहरी विधानों से सीमित हो गई तब वर्ण आदि के भी आंतरिक की बजाय बाहरी मानकों का ही सहारा लेना पड़ा।
इसे हम एक अन्य दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। इसे हम आत्म-तत्व द्वारा उच्चतर से स्थूलतर स्तरों तक के अवरोहण के रूप में, अधिकाधिक स्थूलतर स्तरों तक अभिव्यक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। अभिव्यक्ति के अंदर भगवान् का प्रकाश पहले अंतर्ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है, उसके बाद वह प्रकाश बुद्धि में आता है, उसके बार मानसिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर, स्थूलतर प्राणिक स्तर पर और उसके बाद स्थूल भौतिक स्तर पर आता है। वह प्रकाश, वह परमात्म तत्व जिस भी स्तर पर कार्य करेगा उसी के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति होगी। यह वैसा ही है जैसे यदि कोई परम् विद्वान् शिक्षक भी अधिकाधिक निचले स्तर की कक्षाओं को पढ़ाए तो भले उसमें कितनी भी विद्वत्ता क्यों न हो तो भी उसे बालक की सीमाओं को ध्यान में रखना होता है और उसी के अनुरूप वह अपने ज्ञान को प्रकट करता है। उसी तरह जैसे-जैसे परमात्मा का प्रकाश अधिकाधिक स्थूलतर स्तरों में आता है वैसे-वैसे उसी के अनुरूप उसकी अभिव्यक्ति मर्यादित होती जाती है। इसी अवरोहण के अनुरूप हम अपनी संस्कृति के विभिन्न काल देख सकते हैं। आरंभ में जब अंतर्भासात्मक युग था, तब चूँकि व्यक्ति सहज रूप से आंतरिक सामंजस्य की स्थिति में था इसलिए किन्हीं बाहरी रूपों और व्यवस्थाओं की अधिक आवश्यकता नहीं थी। यह वैदिक काल था। जब आत्मा का प्रकाश इससे कुछ अधिक मानसिक स्तर पर आया तब हम उपनिषद् का काल पाते हैं। इसके पश्चात् जब सत्य का अधिक मानसीकरण हुआ तब वेदों के ही सत्य को छः धाराओं में बाँट कर षड्दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी क्रम में हम स्मृतियों और अनेक योगसूत्रों को पाते हैं। इसके बाद इन सभी पद्धतियों का समन्वय साधने के लिए गीता का प्राकट्य होता है। गीता अपने पूर्व की सभी प्रणालियों, योग पद्धतियों आदि का बड़े ही व्यापक रूप से समन्वय साध देती है। इसके बाद हम अनेक दर्शनों, तंत्रों तथा पुराणों का काल पाते हैं जब सत्ता के अधिकाधिक प्राणिक-भौतिक भागों में उस प्रकाश का अवतरण हुआ। तत्पश्चात् हम कालिदास आदि महान् कवियों का युग पाते हैं जब सुखभोगवादी भागों को भी उस प्रकाश से जोड़ने का प्रयास किया गया। अंत में जब जड़- भौतिक स्तर तक उस प्रकाश को लाने का समय आया तब श्रीअरविन्द व श्रीमाँ ने अतिमानसिक चेतना के अवतरण के द्वारा भौतिक रूपांतर का दर्शन प्रदान किया। इस प्रकार उच्चतम स्तरों से जड़भौतिक तक के
स्तरों तक चेतना के अवतरण की यह एक अटूट श्रृंखला है। [गीता] बाह्य नियम पर बहुत ही कम बल देती है जबकि वह उस आंतरिक विधान पर बहुत अधिक बल देती है जिसे वर्ण व्यवस्था ने विधिवत् अथवा नियंत्रित बाह्य अभ्यास में ढालने का प्रयास किया। इस प्रकरण में इस विधान के समष्टिगत एवं आर्थिक या अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर नहीं, अपितु वैयक्तिक एवं आध्यात्मिक मूल्य पर ही गीता की विचार-दृष्टि जमी हुई है। गीता ने यज्ञ के वैदिक सिद्धांत को स्वीकार किया, परंतु उसने इसे एक गंभीर रूप, एक आंतरिक, आत्मगत एवं वैश्विक अथवा व्यापक अर्थ, एक आध्यात्मिक भाव एवं दिशा प्रदान की जो इसके सभी मूल्यों को बदल डालती है। यहाँ भी यज्ञ-सिद्धांत की ही भाँति यह चार प्रकार के मनुष्यों (बतुर्वर्ण) के सिद्धांत को स्वीकार करती है परंतु इसे एक गंभीर रूप, एक आंतरिक, आत्मपरक और सार्वभौमिक अर्थ, एक आध्यात्मिक भाव और दिशा प्रदान कर देती है। और, उसके ऐसा करने से एकाएक ही इस सिद्धांत के पीछे मूलभूत विचार के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है और वह एक ऐसा स्थायी एवं जीवंत सत्य बन जाता है जो किसी विशिष्ट सामाजिक प्रणाली एवं व्यवस्था के अस्थायित्व से नहीं बँधा होता। गीता जिस चीज से तात्पर्य रखती है वह आर्यों की उस समाज-व्यवस्था की प्रामाणिकता से नहीं है जो अब विलुप्त हो चुकी है या मरणासन्न अवस्था में है, - यदि यही इसका संपूर्ण अभिप्राय होता तो स्वभाव और स्वधर्म के उसके सिद्धांत में कोई स्थायी सत्य या स्थायी मूल्य की बात न होती, - अपितु गीता की रुचि मनुष्य की आंतरिक सत्ता के साथ उसके बाह्य जीवन के संबंध से है, उसकी अंतरात्मा से तथा उसकी प्रकृति के आंतरिक विधान से उसके कर्म के विकास से है।
गीता के संबंध में यही बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है, और इसे जितनी बार दुहराया जाए उतना ही अच्छा है, कि जब वह वर्ण-व्यवस्था या यज्ञ जैसे किसी विषय की चर्चा करती है तब उसका आग्रह केवल उनके बाह्य स्वरूप पर नहीं अपितु उनके आंतरिक विधान पर अधिक होता है। और जिस रूप में गीता अपने विषय को विकसित करती है उससे उसे एक ऐसा व्यापक रूप प्राप्त हो जाता है कि फिर वह कोई सामयिक विषय न रहकर एक सनातन सत्य बन जाता है। गीता के सभी विषयों पर यह बात लागू होती है। गीता के ऐसे स्वरूप को केवल श्रीअरविन्द ने ही अपनी टीका के माध्यम से उजागर किया है अन्यथा तो हम गीता की इस शैली को चूक जाते हैं। गीता में किसी प्रकार की कोई संकुचितता नहीं है। उदाहरण के लिए, गीता जब यज्ञ, तप और दान के विषय में चर्चा करती है, जिन्हें कि सामान्यतः केवल बाह्य क्रियाएँ ही मान लिया जाता है, तब वह इनका सच्चा आंतरिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ और महत्त्व प्रकट करती है, और केवल तभी यह स्पष्ट हो पाता है कि यज्ञ, तप और दान तो ऐसे मूलभूत तत्त्व हैं जो सृष्टि की रचना मात्र में अंतर्निहित हैं और जिन्हें व्यक्ति सचेतन या अचेतन रूप से अवश्य ही करता है। गीता यज्ञ, तप, दान, वर्ण आदि सभी पदों को प्रतीक के रूप में लेती है इसी कारण इन पदों के आंतरिक अभिप्राय को चूकने के कारण व्यक्ति इन्हें केवल बाहरी क्रियाएँ समझ बैठता है। रूपकों और प्रतीकों के प्रयोग के कारण ही वेदों का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ हमारे लिए प्रत्यश्न नहीं होता। जब तक हम प्रतीकों और रूपकों के पीछे छिपे गूढ अर्थ को न देख पाएँ तब तक हम भारतीय संस्कृति के अधिकांश रहस्य को ही चूक जाएँगे। अतः गीता से यदि हम यह अर्थ लगाएँ कि वह किसी प्रकार की कोई सामाजिक व्यवस्था प्रदान कर रही है, तो यह बिल्कुल बेतुकी बात होगी क्योंकि गीता किन्हीं बाहरी व्यवस्थाओं को नहीं अपितु आत्मा के सत्यों को, आध्यात्मिक सत्यों को प्रकट करने का ग्रंथ है। और जब गीता स्वयं ही सभी धर्मों को छोड़कर भगवान् की शरण में जाने की बात कहती है तब उससे भिन्न अर्थ लगाकर हम गीता को किन्हीं बाहरी कर्मों के प्रतिपादन का ग्रंथ कैसे कह सकते हैं या यह अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि वह किन्हीं बाहरी क्रियाओं के रूप में यज्ञ, तप, दान, वर्ण आदि का वर्णन करेगी।
और वास्तव में हम देखते हैं कि स्वयं गीता ही अपने इस आशय को अत्यंत स्पष्ट रूप में दर्शा देती है जब वह ब्राह्मण और क्षत्रिय के कर्म का वर्णन बाह्य कार्यव्यापार की शब्दावली में, शिक्षा, पौरोहित्य एवं शास्त्रालोचन या राज्य-कार्य, युद्ध एवं राजनीति की परिभाषा में नहीं, अपितु सर्वथा, आंतरिक स्वभाव की परिभाषा में करती है। उसकी भाषा हमारे कानों को कुछ विचित्र प्रतीत होती है। शांत-स्थिरता, आत्मसंयम, तपस्या, शुचिता, सहनशीलता, सरल व्यवहार, आध्यात्मिक सत्य की स्वीकृति तथा उसके अभ्यास को साधारणतः मनुष्य का कर्त्तव्य, कर्म या जीवन-व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। तथापि गीता का कथन और तात्पर्य ठीक यही है, वह कहती है कि ये चीजें, इनका विकास, आचार-व्यवहार में इनकी अभिव्यक्ति, सात्त्विक प्रकृति के धर्म को बाह्य रूप में ढालने की इनकी शक्ति ब्राह्मण का वास्तविक कर्म हैः शिक्षा, धार्मिक पौरोहित्य तथा अन्य बाह्य कर्त्तव्य इस कर्म का एक अत्यंत उपयुक्त क्षेत्र मात्र हैं, इस अंतर्विकास का एक अनुकूल साधन, इसकी समुचित आत्म-अभिव्यक्ति, सुस्थिर आदर्श में और चरित्र की बाह्य सुदृढ़ता में अपने को प्रतिष्ठित करने की पद्धति है। युद्ध, शासन-कार्य, राजनीति, नेतृत्व और प्रभुत्व क्षत्रिय के लिए उसी प्रकार का क्षेत्र एवं साधन है: परंतु उसका वास्तविक कर्म है राजोचित या वीरोचित सक्रिय युद्ध-भावना के धर्म का विकास, व्यवहार में उसकी अभिव्यक्ति, बाह्य रूप में तथा ऊर्जस्वी गतिच्छंद में उसे सशक्त रूप में ढालना। वैश्य और शूद्र का कर्म बाह्य कर्तव्य की परिभाषा में व्यक्त किया गया है, और इस विपरीत प्रवृत्ति का कुछ अर्थ हो सकता है। क्योंकि, उत्पादन और धनोपार्जन में प्रवृत्त या श्रम और सेवा के घेरे में आबद्ध प्रकृति, व्यापारिक और दासोचित मनोवृत्ति साधारणतः बहिर्मुखी होती है, अपने कर्म की चरित्र-गठन करने की शक्ति की अपेक्षा उसके बाह्य मूल्य-महत्त्व में ही अधिक ग्रस्त रहती है, और यह स्वभाव प्रकृति के सात्त्विक या आध्यात्मिक कर्म के लिए इतना अनुकूल नहीं है। यह भी एक कारण है जिससे कि एक व्यावसायिक एवं औद्योगिक युग या कर्म और श्रम के विचार में व्यस्त समाज अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बना लेता है जो आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा भौतिक जीवन के अधिक अनुकूल होता है, ऊर्ध्वगामी मन और आत्मा की सूक्ष्मतर पूर्णता की अपेक्षा प्राण की क्षमता के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तथापि, इस प्रकार की प्रकृति और इसके कार्यों का भी अपना आंतरिक अर्थ एवं आध्यात्मिक मूल्य होता है और इन्हें पूर्णता का साधन व शक्ति बनाया जा सकता है। जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है, आध्यात्मिकता, नैतिक पवित्रता और ज्ञान के आदर्श से संपन्न केवल ब्राह्मण ही नहीं, और महत्ता, वीरता एवं चारित्रिक उच्चता के आदर्श से युक्त केवल क्षत्रिय ही नहीं, अपितु अर्थाभिलाषी वैश्य, श्रमपाश में बद्ध शूद्र, संकीर्ण, सीमाबद्ध एवं पराधीन जीवन की भागिनी स्त्री और पाप के गर्भ से उत्पन्न शूद्र, 'पापयोनयः', तक भी इस मार्ग से तुरंत उच्चतम आंतरिक महत्ता एवं आध्यात्मिक स्वाधीनता की ओर उठ सकते हैं, सिद्धि की ओर, मानव-सत्ता के दिव्य तत्त्व की मुक्तावस्था एवं परिपूर्णता की ओर आरोहण कर सकते हैं।
गीता कहीं भी अपनी शिक्षा को बाहरी व्यक्तित्व से या वर्ण से सीमित नहीं करती। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अधम से अधम या पापयोनि में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, सीधे ही आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर उठ सकता है, परमात्मा के पास जा सकता है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी अवस्था व्यक्ति को परमात्मा तक जाने से नहीं रोक सकती। इसी संदर्भ में गीता स्वभाव नियत कर्म का प्रतिपादन करती है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके सीधे ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी शूद्र वर्ण को ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए दिव्य स्वतंत्रता के द्वार उसी वर्ण में खुले हैं। इसी की चेतावनी देते हुए गीता कहती है कि किसी अन्य व्यक्ति के धर्म का भली प्रकार अनुष्ठान भी कल्याणकारी नहीं होता क्योंकि वास्तव में वह तो अपनी ही सत्ता के सत्य का खण्डन है। अपनी सत्ता के सत्य के अनुरूप क्रिया ही व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो सकती है और उसी के द्वारा वह परमात्मा तक पहुँच सकता है। अतः भले कोई किसी भी वर्ण का ही क्यों न हो, उसे अपने अंतर्निहित स्वभाव के अनुसार क्रिया करने पर आध्यात्मिक स्वातंत्र्य प्राप्त हो सकता है। अपने वर्तमान वर्ण के अनुसार क्रिया करते-करते उसमें अवश्य ही यथोचित रूप से अन्य गुणों का भी विकास हो जाता है और वह भगवान् के मद्भाव तक जा सकता है।
प्रश्न : यहाँ दो बातें आई हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक रचना भिन्न-भिन्न है। और दूसरे यह कि अपनी किन्हीं भी बाहरी परिस्थितियों के द्वारा भी व्यक्ति भगवान् की ओर जा सकता है। इन दोनों ही बातों में सामंजस्य कैसे स्थापित करें?
उत्तर : इसी के तालमेल के लिए तो स्वभाव नियत कर्म की व्यवस्था है। व्यक्ति का जो भी आंतरिक ढाँचा है, उसके अनुसार उसे क्रिया करनी चाहिये। हालाँकि क्रिया से गीता का अर्थ हम जिसे प्रचलित रूप से क्रिया कहते हैं वह नहीं है। श्रीअरविन्द की टीका से तो स्पष्ट हो जाता है कि गीता जब ब्राह्मण और क्षत्रिय के कर्मों का वर्णन करती है तब वह भी किन्हीं बाहरी कर्मों के रूप में नहीं अपितु आंतरिक गुणों की परिभाषा में करती है। अतः अपने आंतरिक ढाँचे के अनुसार व्यक्ति अपने बाहरी कर्म कर सकता है और धीरे-धीरे उसमें अन्य सभी वर्णों का भी विकास हो जाता है। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ण को मद्भाव तक पहुँचने में अपने निज स्वभाव के अतिरिक्त अन्य तीन वर्णों के गुणों का भी विकास करना होता है। इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि शुरू में व्यक्ति का वर्ण कौनसा है।
इस प्रकरण पर प्रथम दृष्टिपात करते ही तीन वाद या प्रस्थापनाएँ हमारे सामने स्वयमेव उपस्थित होती हैं और यहाँ गीता ने जो कुछ भी कहा है उस सब में उन तीनों को अंतर्निहित समझा जा सकता है। प्रथम, समस्त कर्म अंदर से ही निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई अपना निज तत्त्व होता है, अपनी प्रकृति का कोई विशिष्ट धर्म एवं सहजात शक्ति होती है...जो उसको प्रकृतिगत अंतरात्मा के क्रियाशील रूप का सृजन करती है और उसे कर्म के द्वारा व्यक्त करना और पूर्ण बनाना, शक्ति-सामर्थ्य, आचार-व्यवहार और जीवन में उसे प्रभावोत्पादक बनाना ही उसका कार्य है, उसका सच्चा कर्म है: वह उसे आंतर और बाह्य जीवनचर्या के उचित मार्ग का निर्देश करती है तथा उसके और आगे के विकास के लिए यथार्थ प्रारंभ-स्थल होती है। दूसरे, मोटे तौर पर मनुष्य की प्रकृति चार श्रेणियों की होती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कर्तव्य, कर्म और स्वभाव का अपना आदर्श नियम है और यह श्रेणी मनुष्य के अपने विशिष्ट क्षेत्र को सूचित करती है और इसी को उसके बाह्य सामाजिक जीवन में उसकी यथार्थ कार्यपरिधि का निर्धारण करना चाहिए। अंत में, मनुष्य चाहे जो भी कर्म करे, यदि वह उसकी सत्ता के धर्म, उसकी प्रकृति के सत्य के अनुरूप किया जाए तो उसे ईश्वरोन्मुख मोड़ा जा सकता है और आध्यात्मिक मुक्ति एवं सिद्धि का एक कारगर साधन बनाया जा सकता है। इनमें से प्रथम और अंतिम प्रस्थापनाएँ एक प्रत्यक्ष सत्य एवं धर्मपरायणता की द्योतक हैं। निःसंदेह मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनचर्या का सामान्य ढंग इन सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतीत होता है; क्योंकि निश्चय ही हम अपने ऊपर बाह्य आवश्यकता, नियम और विधान का भयानक बोझ वहन करते हैं, और आत्म-अभिव्यक्ति की, जीवन में अपने सच्चे व्यक्तित्व, अपनी सच्ची आत्मा, अपने अंतरतम विशिष्ट स्वधर्म के विकास की हमारी आवश्यकता को पारिवेशिक प्रभाव द्वारा हर मोड़ पर बाधाग्रस्त किया जाता है, व्याघात पहुँचाया जाता है, बलपूर्वक अपने पथ से च्युत कर दिया जाता है, अथवा बहुत ही क्षीण अवसर और तुच्छ विस्तार-क्षेत्र प्रदान किया जाता है। प्रतीत होता है कि जीवन, राष्ट्र, समाज, परिवार और हमारे चारों ओर की सभी शक्तियों ने हमारी आत्मा पर अपना जुआ लादने के लिए, अपने साँचों में हमें बलात् ढालने के लिए, हम पर अपना यांत्रिक स्वार्थ और स्थूल तात्कालिक सुख-साधन थोपने के लिए षड़यंत्र कर रखा है। हम मशीन के पुर्जे बन जाते हैं; हम सच्चे अर्थों में मनुष्य, 'पुरुष', आत्मा और मन नहीं होते हैं, आत्मा की ऐसी मुक्त संतति, ऐसे अमृत पुत्र नहीं होते हैं जो अपनी सत्ता की उच्चतम स्वभावगत पूर्णता का विकास करने और उसे जाति की सेवा का साधन बनाने में समर्थ हों और कदाचित् ही हमें सच्चे अर्थों में ऐसे बनने के लिए अवसर ही दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होगा कि हम वैसे नहीं होते जैसा हम अपने को बनाते हैं, अपितु वैसे होते हैं जैसा हमें बनाया जाता है। परंतु फिर भी, जितना अधिक हम ज्ञान में अग्रसर होंगे, उतना है अधिक गीता के विधान का सत्य हम पर अवश्यमेव ही प्रकट होगा। बालिक को शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसकी प्रकृति के अंदर जो कुछ जी कने श्रेष्ठ, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत अंतरंग और जीवंत है वह सब बाहर प्रकट हो जाए; मनुष्य के कर्म और विकास को जिस साँचे में ढलना चाहिए वह उसके स्वभावगत गुण और सामर्थ्य के अनुरूप ही होना चाहिए। नयी चीजें उसे अवश्य प्राप्त करनी होंगी, पर उन्हें वह, सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत प्राणवंत रूप में, अपने ही विकसित किये आदर्श तथा सहजात शक्ति के आधार पर ही प्राप्त कर सकेगा। और, इसी प्रकार मनुष्य के कर्तव्य उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, प्रतिभा और क्षमताओं के द्वारा ही निर्धारित होने चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार स्वतंत्र रूप से विकसित होगा वह एक जीवंत आत्मा और मन होगा और उसके अंदर जाति की सेवा के लिए कहीं अधिक महत्तर शक्ति होगी। और, अब हम अधिक स्पष्ट रूप में यह देख सकते हैं कि यह नियम केवल व्यक्ति के संबंध में ही नहीं, अपितु समाज और राष्ट्र, सामुदायिक आत्मा एवं समष्टिगत मानव के संबंध में भी सत्य है। चार वर्णों तथा उनके कार्यों के संबंध में दूसरा मत अधिक विवादास्पद है। यह कहा जा सकता है कि यह अत्यंत सीधा-सादा और निश्चयात्मक है, कि यह जीवन की जटिलता और मानव-प्रकृति की नमनशीलता को पर्याप्त रूप से विचार में नहीं लाता, और सिद्धांत या उसकी अंतर्निहित विशेषताएँ कुछ भी क्यों न हों, उसका बाह्य सामाजिक प्रयोग यांत्रिक आचार के ठीक उसी अत्याचार की ओर ले जाएगा जो स्वधर्म के समस्त विधान के सर्वथा विरुद्ध है। परंतु ऊपरी सतह के नीचे इसका एक गंभीरतर अर्थ भी है जो इसे एक कम संदिग्ध मूल्य प्रदान करता है। और, चाहे हम इसे अस्वीकार भी कर दें, फिर भी तीसरा मत अपने व्यापक अर्थ को लिए हुए अटल रहेगा। जीवन में मनुष्य का कर्म एवं कर्तव्य कोई भी क्यों न हो, यदि वह कर्म अंदर से निर्धारित हो अथवा यदि मनुष्य को ऐसा अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह उस कर्म को अपनी प्रकृति की आत्म-अभिव्यक्ति बना सके तो वह उसे विकास तथा महत्तर आंतरिक पूर्णता का साधन बना सकता है। और, उसका स्वाभाविक कर्म कोई भी क्यों न हो यदि वह उसे उचित भावना में संपन्न करे, आदर्श मन के द्वारा उसे आलोकित कबरे यदि वह उसकी क्रिया को अपने अंतःस्थ भगवान् के उपयोग में लगा है, विश्व में अभिव्यक्त परमात्मा की उसके द्वारा सेवा करे अथवा मानवता में भगवान् के जो उद्देश्य हैं उनके लिए उसे एका सयेता कये करण बना दे तो वह उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक पूर्णता और स्वतंत्रता के साधन के रूप में परिणत कर सकता है।
यहाँ जो तीन बातें हैं उनमें पहली यह है कि हमारी समस्त शिक्षा, हमारे कर्म, आचार-व्यवहार आदि सभी कुछ एकमात्र हमारे आन्तरिक सत्य को ही विकसित और अभिव्यक्त करने के साधन होने चाहिये। परन्तु वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमारी अंतरात्मा पर बाहरी जीवन के नियमों, परिवार, जाति, समाज, राष्ट्र आदि के विधानों, भौतिक विज्ञान के नियमों आदि के अनेकानेक जुए लदे रहते हैं जिनके कारण उसे सहज रूप से अपने-आप को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता। दूसरी बात यह है कि मनुष्यों की प्रकृति की चार श्रेणियाँ होती हैं और प्रत्येक मनुष्य का अपनी ही श्रेणी के अनुसार विशिष्ट कर्त्तव्य, कर्म और स्वभाव होता है और इसी के अनुसार सामाजिक जीवन में उसकी व्यावहारिक भूमिका निर्धारित होनी चाहिये। इसमें तीसरी बात जो सबसे महत्त्वपूर्ण है वह यह है कि व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, हमारे बाहरी कर्म का स्वरूप जो भी क्यों न हो परंतु ये सभी अंतरात्मा की अभिव्यक्ति के साधन बन सकते हैं। मूलतः जिन्हें हम बाहरी परिस्थितियाँ कहते हैं वे भी परम् प्रज्ञा द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं और जाने-अनजाने वे सभी हमें आगे की ओर ले जाती हैं। परंतु अज्ञानवश मनुष्य बाहरी परिस्थितियों को, अपने परिवेश को, दूसरे लोगों को, वातावरण को, समाज को या फिर उसे मिली बाहरी प्रकृति को ही कोसता है कि वे उसकी प्रगति में बाधक हैं। या फिर व्यक्ति भाग्य को कोसता है कि उसे दुर्भाग्यवश प्रगति के सुअवसर प्राप्त नहीं हुए। परंतु ये सभी केवल बहाने मात्र हैं। यदि कोई वास्तव में परमात्मा की ओर जाना चाहे तो सारे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो उसे उस ओर जाने से रोक सके। इस संदर्भ में श्रीमाताजी कहती हैं, "कभी मत कहो कि 'अमुक व्यक्ति यह नहीं करता,' 'अमुक व्यक्ति तो कुछ और ही चीज करता है,' 'कि वह तो वही करता है जो उसे नहीं करना चहिये' - इन सब बातों से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। तुम इस पृथ्वी पर, एक भौतिक शरीर में, एक सुनिश्चित उद्देश्य से लाये गये हो और वह उद्देश्य है इस शरीर को जितना संभव हो उतना सचेतन बनाना, इसे भगवान् का अत्यंत पूर्ण और अत्यंत सचेतन यंत्र बनाना। भगवान् ने तुम्हें चेतना के सभी क्षेत्रों में - मानसिक, प्राणिक और भौतिक क्षेत्र में - वह तुमसे जो कुछ आशा करते हैं उसके अनुपात में योग्यता और साधन की एक विशेष मात्रा प्रदान की है, और वह जो कुछ तुमसे आशा रखते हैं उसी के अनुपात में तुम्हारे चारों ओर की समस्त परिस्थितियाँ भी व्यवस्थित हैं, और जो लोग तुमसे यह कहते हैं, 'मेरा जीवन भयावह है, मैं संसार में अत्यंत दयनीय जीवन यापन करता हूँ,' वे गधे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन ऐसा है जो उसके सर्वांगपूर्ण विकास के उपयुक्त है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अनुभव प्राप्त हैं जो उसे उसके सर्वांगपूर्ण विकास में सहायता देते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख जो कठिनाइयाँ हैं वे भी ऐसी हैं जो उसे उसकी पूर्ण उपलब्धि में सहायता देती हैं।
यदि तुम अपनी ओर सावधानी के साथ दृष्टिपात करो तो देखोगे कि तुम सर्वदा ही अपने अन्दर उस सद्गुण के विपरीत वस्तु को वहन करते हो जो तुम्हें उपलब्ध करनी है (यहाँ मैं "सद्गुण" शब्द का प्रयोग उसके विशालतम और उच्चतम अर्थ में कर रही हूँ।) तुम्हारा एक विशेष लक्ष्य है, एक विशेष उद्देश्य है, एक विशेष उपलब्धि है, जो तुम्हारी अपनी है, हर एक की व्यक्तिगत, और तुम अपने अंदर अपनी उपलब्धि को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक सभी कठिनाइयों को वहन करते हो। सर्वदा ही तुम यह देखोगे कि तुम्हारे अन्दर अंधकार और प्रकाश समान-रूप से हैं : तुममें एक योग्यता है, तुममें उस योग्यता का अभाव भी है। परंतु तुम यदि अपने अंदर एक बहुत काला छिद्र, बहुत घना अंधकार देखो तो यह निश्चित रूप से जानो कि तुम्हारे अंदर कहीं पर एक महान् प्रकाश भी है। अब यह तुम्हारा काम है कि तुम यह जानो कि एक का उपयोग दूसरे की संसिद्धि के लिये किस प्रकार किया जाए।" (CWM 4,117-18)
श्रीमाताजी के वचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में यदि कोई कुछ करना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। सारे ब्रह्माण्ड में ऐसा कुछ नहीं जो किसी व्यक्ति को प्रगति करने से रोक सकता हो क्योंकि वास्तव में उसकी प्रगति के अनुकूल ही तो सारा ब्रह्माण्ड बना है। ऐसी कोई बाहरी घटना, कोई बाहरी परिस्थिति या अन्य कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो व्यक्ति की प्रगति को रोक सकता हो। इसीलिए गीता का यह सिद्धांत कि किन्हीं भी बाहरी चीजों को आंतरिक अभिव्यक्ति का साधन बनाया जा सकता है, एक परम् सिद्धांत है। जब सच्चाई का अभाव हो केवल तभी व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर दोषारोपण करता है। यहाँ तक कि दासता की स्थिति भी व्यक्ति को भगवान् के पास पहुँचने से नहीं रोक सकती। सूफी संत राबिया के जीवन वृत्तांत से हम देखते हैं कि किस प्रकार माता-पिता के देहांत के बाद भयंकर अकाल के समय किसी क्रूर व्यक्ति ने उसे कुछ पैसों के लिए अन्य किसी व्यक्ति को गुलाम के रूप में बेच दिया। जब राबिया अपने मालिक के घर में पहुंची तब उसे सारे दिन काम करना पड़ता। परंतु रात के समय वह प्रभु की इबादत करते हुए उनके प्रेम में रोती रहती थी। एक रात उसके रोने की आवाज सुनकर जब उसके मालिक ने उसकी स्थिति देखी और उसके चारों ओर के अद्भुत प्रकाश को देखा तो वह अवाक् रह गया और भीतर से द्रवित हो उठा और तुरंत ही उसने उसे मुक्त कर दिया। कहने का अर्थ है कि यदि भीतर सच्चाई हो तो बाहर से गुलामी की अवस्था भी व्यक्ति को प्रभु से मिलने से नहीं रोक सकती। यदि हम सच्चाई के साथ सभी चीजों से मुक्त होना चाहें तो ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें रोक सके। अतः परिस्थितियों को हम दोष भले ही देते हों, परंतु वास्तव में तो हमें अपनी उस स्थिति में बड़ा सुख मिलता है और हम उस अंधकार से निकलना चाहते ही नहीं। गीता हमें उसी अंधकार से निकालने का प्रयास करती है। वह कहती है कि एक बार जब व्यक्ति के यह समझ में आ जाए कि केवल परमात्मा ही एकमात्र पाने योग्य हैं तब उसे उनकी प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता और वह उन्हें अवश्य ही प्राप्त करके रहेगा। गीता के अनुसार किसी अधम या नीच या अत्यंत दुराचारी व्यक्ति में भी यदि यह संकल्प आ जाता है तो वह भी साधु मानने योग्य है जो कि अपने सारे कुल का भी कल्याण कर देता है, वहीं कोई सात्त्विक ब्राह्मण जो भगवान् की भक्ति से शून्य है, वह स्वयं अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। अतः गीता की शिक्षा भी किसी प्रकार की शिकायत के लिए कोई स्थान नहीं देती।
एक चीज जो हमें सदा ध्यान में रखनी चाहिये वह यह है कि गीता की दूसरी प्रस्थापना का, अर्थात् चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत का, हम बाकी दो प्रस्थापनाओं से पृथक् करके विचार नहीं कर सकते। क्योंकि गीता का मत मूल रूप से यही है कि व्यक्ति की अंतरात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव होनी चाहिये और उसी के अनुसार उसके बाहरी कर्म निर्धारित होने चाहिये। इस सहज अभिव्यक्ति में सामान्यतः बाह्य सामाजिक और व्यक्तिगत नियम बाधा डालते हैं, हालाँकि उसका भी अपना एक गहन और गुह्य कारण है, परंतु जब तीसरी प्रस्थापना विद्यमान है, कि किसी भी 'बाहरी परिस्थिति के अंदर भी व्यक्ति सीधे प्रभु के पास पहुँच सकता है. तब फिर तत्त्वतः तो कोई समस्या ही नहीं रहती। यदि व्यक्ति के भीता आत्मा का प्रकाश है तो ऐसी कोई बाहरी शक्ति नहीं जो उसे प्रस्थायि होने से रोक सके। जब व्यक्ति में परमात्मा के प्रति लगन लग गई तब किसी भी बाहरी परिस्थिति में क्या सामर्थ्य हो सकती है कि उसे रोक सके। जब व्यक्ति भीतर से माँ जगदंबा की शरण में हो, जिनकी विना इच्छा के कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता, तब फिर किसी प्रकार के अनिष्ट की क्या संभावना है? परंतु हमारा अहं इस पर हमें विश्वास नहीं करने देता। वहीं, ज्यों-ज्यों भीतर से हमारा ज्ञान बढ़ता है त्यों-त्यों हम पाते हैं कि परिस्थितियाँ तो कभी रुकावट बन ही नहीं सकतीं अपिन के तो हमारी प्रगति के लिये आवश्यक साधन अथवा यंत्र हैं। सही चेतना में परिस्थितियाँ तो व्यक्ति को अवरोध की बजाय अवलंब सिद्ध होती हैं। जितना ही हम चैतन्य होंगे उतना ही अधिक हमें वे साधन के रूप में नजर आएँगी न कि हमारे ऊपर लादे गये जुए के रूप में। इस सत्य को भगवान् गीता में भिन्न-भिन्न तरीकों से स्थापित करते हैं।
श्रीअरविन्द के अनुसार यदि चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत को इस अंतिम प्रस्थापना से समन्वित करके न देखा जाए तो हम गीता की शिक्षा के मूल स्वरूप को ही विकृत कर देंगे। आरंभ से ही हम यह देखते आए हैं। कि जो विषय गीता में बिल्कुल गौण और देश-काल से सीमित प्रतीत होते हैं वे भी अपने गहरे अर्थ में लेने पर अपना वह स्वरूप छोड़ कर व्यापक स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार हमें यह समझ लेना चाहिये कि गीता कभी भी जाति-प्रथा जैसी किसी सीमित चीज का प्रतिपादन नहीं कर सकती अतः हमें इसे इसके व्यापक स्वरूप में लेने पर हो इसका सही अर्थ समझ में आ सकता है।
प्रश्न : यहाँ टीका में श्रीअरविन्द कहते हैं कि, "यह नियम केवल व्यक्ति के संबंध में ही नहीं, अपितु समाज और राष्ट्र, सामुदायिक आत्मा एवं समष्टिगत मानव के संबंध में भी सत्य है।" इसका क्या अर्थ है?
उत्तर : इसका अर्थ है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए यह लागू होता है कि उसके भीतरी स्वभाव के अनुसार उसके बाहरी कमों का निर्धारण होना चाहिये ताकि उसकी अंतरात्मा की सहज अभिव्यक्ति हो सके, उसी प्रकार यह बात समष्टिगत आत्मा पर भी लागू होती है। किसी समाज का, किसी राष्ट्र का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है और उसकी अपनी आत्मा होती है जिसे अपनी अभिव्यक्ति का उतना ही उसविकार है जितना किसी व्यक्ति को। श्रीअरविन्द व स्वामी विवेकानंद, धोनों ने ही अनेकों स्थानों पर इस सत्य को उजागर किया है। पद, याचियात्मिकता ही भारत का अंतर्निहित भाव है, उसकी आत्मा है और यदि इस आत्मा की अवहेलना कर हम पाश्चात्य संस्कृति के मूल्यों को भारत की आत्मा पर लादने का प्रयास करें तो इसका परिणाम सर्वनाश होगा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, "यदि तुम उस आध्यात्मिकता को छोड़कर पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के पीछे जाओगे, तो इसका परिणाम यह होगा कि तुम तीन ही पीढ़ियों में लुप्त जाति बन जाओगे; क्योंकि इससे जाति की मेरुदण्ड ही टूट जाएगी, और जिस आधार पर विराट् राष्ट्रीय भवन बनाया गया है, वह नष्ट हो जाएगा; और इसका परिणाम होगा हर तरह से संपूर्ण सर्वनाश।" (CWSV 3, 151-53)
प्रश्न : एक स्थान पर श्रीअरविन्द यहाँ कहते हैं कि प्रतीत होता है कि अनेकानेक बाहरी शक्तियों ने अपना जुआ हमारे ऊपर थोप कर हमें यंत्रवत् चलाने का षड़यंत्र रच रखा है जिससे कि हम कोई आत्मा या 'पुरुष' न रह कर मशीन के पुर्जों की भाँति व्यवहार करने लगते हैं। और इसके लिए ज्ञान को इससे छूट निकलने का उपाय बताया गया है। इस सारे विषय का अभिप्राय क्या है?
उत्तर : प्रत्येक व्यक्ति की अन्तरात्मा का अपना एक सत्य है। इस आंतरिक सत्य की अभिव्यक्ति के लिये हमारी बाहरी सत्ता का निर्माण होता है। परन्तु यहाँ जिस आंतरिक सत्य की बात हो रही है वह तो केवल व्यष्टिगत अभिव्यक्ति और उसके सत्य की बात है जबकि परमात्मा केवल व्यष्टिगत ही नहीं अपितु वैश्विक और परात्पर भी हैं। अतः व्यक्ति केवल व्यष्टिगत अभिव्यक्ति से ही सीमित नहीं है, वैश्विक और परात्पर भी उसी के पहलू हैं। इस दृष्टिकोण से जो कुछ भी व्यष्टिगत और समष्टिगत अभिव्यक्ति हुई है वह सब कुछ व्यक्ति स्वयं ही है, और वह स्वयं ही परात्पर भी है। इस पहलू को हमें सदा ही ध्यान में रखना चाहिये। अतः यहाँ जिस सत्य की अभिव्यक्ति की बात है वह तो केवल व्यष्टिगत सत्य की अभिव्यक्ति की बात है। परंतु व्यक्ति केवल इसी से सीमित नहीं हो जाता चूंकि वैश्विक और परात्पर भी उसी की सत्ता के पहलू हैं। अब वैश्विक पहलू में सभी समष्टियाँ सम्मिलित हो जाती हैं और व्यष्टिगत विकास के साथ ही साथ समष्टिगत विकास भी चल रहा है। गीता में जो चर्चा है वह तो केवल व्यष्टिगत सत्य की बात है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कि हम शरीर के किसी अंग विशेष के सत्य की बात कर रहे हों। अतः जब तक उस अंग विशेष की बात हो तब तक तो वह सत्य लाग होता है परंतु जब हम पूरे शरीर की बात करें तो उस पर वह उसी प्रकार लागू नहीं हो सकता क्योंकि वह अंग एक बृहत्तर समष्टि का एक भाग है जिसका अपना विधान है। इस दृष्टिकोण से, असंख्यों ब्रह्माण्ड और अनंत स्तरीय अभिव्यक्ति भी हम स्वयं ही हैं। अतः इन सभी पहलुओं को सम्मिलित रूप से लेने पर ही हमारी सत्ता का पूर्णतर सत्य प्रकट हो सकता है। और जब हम उस सत्य को चूक जाते हैं तभी हमें यह प्रतीत होता है कि समाज, राष्ट्र आदि का विधान हमारे ऊपर लादा गया है। श्रीअरविन्द इस विषय को अन्य स्थानों पर तो स्पष्ट करते हैं परंतु गीता के संदर्भ में हम यह आशा नहीं कर सकते कि वे विषय को छोड़कर अन्य तात्त्विक विषयों का निरूपण करने लगेंगे। परंतु अपनी कृति 'मानव-चक्र' में श्रीअरविन्द इस विषय पर प्रकाश डालते हैं कि जिस प्रकार मानव व्यक्तित्व होता है उसी प्रकार किसी जाति, समाज, राष्ट्र आदि समष्टियों का भी अपना-अपना पृथक् व्यक्तित्व होता है और उन सब का भी क्रमविकास चल रहा है और वे भी अपनी अधिकाधिक आत्म-अभिव्यक्ति का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं पृथ्वी की अपनी एक पृथक् सत्ता है, सौर-मंडल की अपनी पृथक् सत्ता है। इस प्रकार इन सारी सत्ताओं का एक ही साथ विकास चल रहा है। यही नहीं, इन असंख्यों भौतिक ब्रह्माण्डों के अतिरिक्त अधिकाधिक सूक्ष्मतर प्राणिक, मानसिक और आंतरात्मिक जगत् हैं वे सब भी व्यक्ति में निहित हैं। अतः अभिव्यक्ति में अंत परिणाम उन सभी की क्रिया के समीकरण के अनुसार होता है। और चूंकि स्वयं परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहे हैं इसलिए प्रतीति भले कुछ भी हो, परंतु सभी चीजें बिल्कुल पूर्ण और समुचित रूप से ही चल रही हैं। जिन्हें हम विषम या प्रतिकूल परिस्थितियों की संज्ञा देते हैं, वे भी वास्तव में तो पूर्ण अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से सहायक ही नहीं अपितु आवश्यक होती हैं। इसलिए ज्यों-ज्यों ज्ञान का विकास होता है त्यों-ही-त्यों व्यक्ति सभी बाहरी परिस्थितियों आदि को अपनी अभिव्यक्ति का साधन बना सकता है। चूँकि परमात्मा असीम हैं, अतः वे बुद्धि से सर्वथा परे हैं। ज्ञान और कुछ नहीं अपितु परमात्मा के किसी तत्त्व को देखने का एक दृष्टिकोण मात्र ही है क्योंकि बुद्धि की पकड़ में आने के बाद तो वह तत्त्व सीमित हो जाता है इसीलिए परमात्मा विस्तृतम और सूक्ष्मतम बुद्धि की पकड़ से भी अनंततः परे हैं। अतः ज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही अधिक परिधि में वह देख सकता है। परंतु वही पूर्ण सत्य नहीं होता। इसीलिए अंत में भगवान् अर्जुन को परम् वचन कहते हैं कि सभी धर्मो का परित्याग कर उनकी शरण ग्रहण कर, क्योंकि अंततः बड़े से बड़ा ज्ञान, बड़े से बड़ा दर्शन भी सीमित ही होता है और भगवान् की उपलब्धि के बीच एक बाधा होता है। इसी कारण भगवान् जगह-जगह पर ज्ञान को नहीं अपितु प्रेम और भक्ति को ही परम् स्थान प्रदान करते हैं। अतः यदि हृदय में भगवान् के लिए प्रेम हो तब फिर चिंता का तो कोई विषय ही नहीं रह जाता। तब ऐसी कोई चीज नहीं रह जाती जो व्यक्ति को भगवान् तक पहुँचने से रोक सके।
जहाँ तक वर्णों की बात है तो यह तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जगदंबा की चार शक्तियों के प्रभाव के कारण ही ये चारों उत्पन्न होते हैं। साथ ही, इसमें अनेक बार इस उक्ति से कुछ भ्रम पैदा हो जाता है कि 'जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् द्विज उच्यते'। इस उक्ति का चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। यह एक मूल सत्य है कि जन्म से तो सभी शूद्र अर्थात् निम्न चेतना में जन्म लेते हैं, केवल संस्कार, अर्थात् शिक्षण, के द्वारा ही उनका नवजन्म साधित होता है। इसी संदर्भ में यह उक्ति प्रचलित थी कि शूद्र को वेदपाठ का अधिकार नहीं है। ऐसा किसी शूद्र वर्ण के संबंध में नहीं कहा जाता था अपितु शूद्र अर्थात् छोटी चेतना के व्यक्ति के संबंध में था जिसे कि वेदपाठ का अधिकारी नहीं समझा जाता था। यह एक स्पष्ट सी बात है कि हम किसी बच्चे के हाथ में घातक हथियार नहीं थमाएँगे। उसी प्रकार एक छोटी चेतना के व्यक्ति द्वारा वेदपाठ संभव नहीं है क्योंकि ऐसा करके वह स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए विभ्रम या संकट की स्थिति पैदा कर सकता है। इसी वर्ण व्यवस्था को समझने का एक और भी गहरा और सूक्ष्म तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये चारों ही वर्ण होते हैं। अपनी आंतरिक सत्ता में सभी द्विज होते हैं और अपनी स्थूल भौतिक चेतना में सभी शूद्र होते हैं। इस तरह शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी अपनी आंतरात्मिक सत्ता में द्विज होता है और वर्ण से ब्राह्मण होने पर भी अपनी स्थूल भौतिक सत्ता में व्यक्ति शूद्र होता है। और इस योजना में प्राण और मन में क्षत्रिय और वैश्य के लक्षण होते हैं। प्राण और मन के अंदर हम लेन-देन, आपसी आदान-प्रदान आदि वैश्य के गुण भी देखते हैं, तो साथ ही साहस, शौर्य, सत्य के लिए संघर्ष आदि कुछ क्षत्रिय संबंधी वृत्तियाँ भी देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की सत्ता के कोषों में इन चारों ही वर्णों के लक्षण होते हैं और चारों का ही विकास करना और उन्हें परमात्मा की ओर मोड़ना आवश्यक है। व्यक्ति परमात्मा की ओर अपने मन, प्राण और शरीर के द्वारा ज्ञानयोग, भक्तियोग या कर्मयोग में से किसी एक के द्वारा या फिर सभी की एक साथ क्रिया द्वारा जा सकता है। और जब वह अंतरात्मा के द्वारा उनको ओर उन्मुख होता है तो यह आध्यात्मिक योग हो जाता है। अतः हम वर्णों से यह अर्थ भी लगा सकते हैं। जब हम इस रूप में गीता को समझें तो पाएँगे कि गीता का अर्थ अत्यंत गंभीर और व्यापक है और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई संकीर्णता प्रतीत होती है तो वह भी केवल हमारे दृष्टिकोण की ही संकीर्णता है, न कि स्वयं गीता की। क्योंकि गीता की शिक्षा किसी देश या काल से सीमित नहीं है अपितु अपने-आप में वह सनातन है और सदा-सर्वदा प्रासंगिक रहती है।
परंतु यदि इस शिक्षा को हम स्वतः-संपूर्ण अर्थ रखने वाले एक स्वतंत्र उद्धरण के रूप में न लें, जैसा कि बहुधा किया जाता है, अपितु सारे ग्रंथ में और विशेषकर अंतिम बारह अध्यायों में वह जो कुछ कहती आ रही है उसके साथ संबंध में इसे देखें, जैसा कि हमें करना ही चाहिए तो गीता की शिक्षा का अर्थ यहाँ और भी गंभीर है। जीवन और कर्मों के विषय में गीता का दर्शन यह है कि सब कुछ भागवत् सत् से, विश्वातीत और विश्वगत परमात्मा से उद्भूत होता है।.... और यद्यपि विश्व की यह परम् आत्मा, यह 'एकमेव' जो सर्व है, हमें माया की शक्ति के द्वारा यंत्रारूढ़ की भाँति संसार-चक्र पर घुमाता हुआ प्रतीत होता है, किसी कुशल यांत्रिक नियम के द्वारा हमें हमारे अज्ञान में उसी प्रकार गढ़ता दिखायी देता है जैसे कुम्हार एक घड़े को गढ़ता है अथवा जैसे जुलाहा कपड़ा बुनता है, परंतु फिर भी यह आत्मा हमारी अपनी हो महत्तम आत्मसत्ता है, और हमारी सत्ता का जो वास्तविक भाव, हमारा अपने आप का जो सत्य है, जो हमारे अंदर विकसित हो रहा है और जन्म-जन्मांतर में नित नये और अधिक उपयुक्त रूप खोज रहा है, हमारे पशु, मानव और दिव्य जीवन में, जो कुछ हम थे, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हम होंगे उस सब में हमारे अंदर विकसित हो रहा है, उसके अनुसार, - उस आंतरिक आत्मिक सत्य के अनुसार हमारी यह अंतरस्थ आत्मा अपनी सर्वज्ञानमय सर्वशक्तिमत्ता में हमें उत्तरोत्तर गठित करती है, जैसा कि हमारी आँखें खुल जाने पर हमें पता लग जाएगा। अहं की यह मशीनरी, त्रिगुण, मन, देह, प्राण, भावावेग, कामना, संघर्ष, विचार, अभीप्सा और प्रयास की यह उलझी हुई जटिलता, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, प्रयास और सफलता-विफलता, जीव और परिवेश, स्व और पर की यह परस्पर-ग्रथित क्रिया-प्रतिक्रिया तो मेरे अंदर की एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति का केवल एक बाह्य अपूर्ण रूप है; अपनी आत्मा में मैं निगूढ़ रूप से जो दिव्य और महान् सत्ता हूँ तथा अपनी प्रकृति में मैं प्रकट रूप से जो दिव्य और महान् सत्ता बनूँगा उसी की आत्म-अभिव्यक्ति को उत्तरोत्तर साधित करने के लिए वह आध्यात्मिक-शक्ति अपने सभी उतार-चढ़ावों के बीच निरंतर यत्न करती है। यह क्रिया अपनी सफलता का तत्त्व अपने-आप के भीतर निहित रखती है, और वह है स्वभाव और स्वधर्म का तत्त्व।
प्रत्येक जीव भगवान् का एक विशेष भाव, एक विशेष पहलू है और उसी के अनुरूप भगवान् उसकी बाह्य प्रकृति को गढ़ रहे हैं। वह विशिष्ट भाव ही स्वभाव है और उसे संसिद्ध करना स्वधर्म है। यह आत्म-अभिव्यक्ति एक आध्यात्मिक तत्त्व है। इसका किसी सामाजिक क्रिया से, जातिगत ऊँच-नीच से कोई संबंध नहीं है। गीता का स्वभाव और स्वधर्म तो व्यक्ति का वह विशिष्ट आंतरिक विधान है जिसके अनुसार भगवान् उस व्यक्ति को अग्रसर करते हैं। जब गीता स्वभाव की बात करती है तब उसका किसी प्रकार की वर्ण-व्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता। वह तो बहुत ही गहरी चीज होती है। साथ ही, अंतर्निहित सभी स्वभावों को एक-एक कर के सर्वांगीण रूप से विकसित करने पर व्यक्ति मद्भाव में पहुँच जाता है। क्योंकि आखिर व्यक्ति स्वयं परमात्मा ही तो है। इसलिए वास्तव में जो वह है वही अंततः उसे बनना है। इस दृष्टिकोण से देखने पर ही हमें इस बात का भान होता है कि गीता किन्हीं सतही विषयों की चर्चा नहीं करती अपितु अकल्पनीय रूप से व्यापक और गहरे तत्त्वों का निरूपण करती है परंतु चूंकि जिन रूपकों या प्रतीकात्मक शब्दों का वह प्रयोग करती है उनको उनके स्थूल अर्थ में लेने पर ही हमें इसकी शिक्षा सतही प्रकार की प्रतीत होती है और हम इसके गंभीर अर्थ को चूक जाते हैं। जिस रूप में अब गीता ने स्वभाव और स्वधर्म को परिभाषित किया है उसमें तो किसी प्रकार के कोई जातिगत विभाजन आदि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वह तो गहन आंतरात्मिक जगतों का विषय है और केवल अनुभूति से ही समझ में आ सकता है। सभी विषयों का धीरे-धीरे विकास करके और कहीं भी न रुकते हुए गीता हमें अब यहाँ ले आई। कि जिन किन्हीं भी साधना आदि की चर्चा हम कर आए हैं वे एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से तो सही हो सकती हैं, परंतु मूल सत्य यह है कि स्वयं परमात्मा ही अपने-आप को इस अभिव्यक्ति में गढ़ रहे हैं। इस अभिव्यक्ति की प्रक्रिया की यदि हमें कोई शैली प्रतीत होती है तो हम उसे किसी योग-पद्धति आदि का नाम दे देते हैं। परंतु वास्तव में परमात्या अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं और किन्हीं भी दो चीजों या व्यक्तियों में अभिव्यक्ति का जो क्रम वे अपनाते हैं वह सर्वथा भिन्न होता है। इस तरह से देखने पर तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सारा जगत्-प्रपंच तो परमात्मा और उनकी पराशक्ति की क्रीड़ा मात्र है। इसमें न किसी प्रकार के कोई वर्ण-विभाजन हैं, न किसी प्रकार की अन्य कोई पद्धति है, न किसी प्रकार का कोई इंद्रियगोचर या आत्मपरक विषय है। श्रीअरविन्द की टीका ही गीता के तत्त्व को उसकी पराकाष्ठा तक ले जाती है अन्यथा तो गीता की शिक्षा को अधिकांशतः किन्हीं मानसिक सूत्रों या कर्म के नैतिक विधानों आदि से अधिक आगे ले जाया ही नहीं जाता। यह तो स्पष्ट ही है कि जो गीता अपनी ऊँची से ऊँची शिक्षा का भी अंत में अतिक्रमण कर जाती है और सभी आधारों, विधानों, शास्त्रों, योग-पद्धतियों आदि को सर्वथा त्याग कर एकमात्र भगवान् को पूर्ण समर्पण करने की बात करती है उसे हम किन्हीं भी सामाजिक नियमों से कैसे बाँध सकते हैं। वह तो हमारे सभी मानसिक धर्मों का पूर्णरूपेण परित्याग करके उन्मुक्त रूप से आत्मा के जगतों में उड़ान भरने की बात करती है, ऐसे ग्रंथ से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वह हमारे किन्हीं भी मानसिक नियमों के तुच्छ दायरे में समा जाए? अतः हमें गीता को उसी के शब्दों में और जो विकासक्रम वह अपनाती है उससे जो सहज अर्थ निकल कर आता है, उसी के प्रकाश में समझने का प्रयास करना चाहिये तभी हम उससे कुछ ग्रहण कर सकते हैं अन्यथा तो अधिकांशतः हम उसमें केवल स्वयं अपनी ही बनी बनाई धारणाओं या पूर्वाग्रहों को पढ़ रहे होते हैं।
और सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि उच्चतम आध्यात्मिक प्रकृति में स्वभाव का एक अर्थ होता है और त्रिगुण की निम्न प्रकृति में वह एक सर्वथा दूसरा ही रूप और अर्थ ले लेता है। वहाँ भी यह क्रिया तो करता है, पर अपने स्वरूप पर इसका पूर्ण अधिकार नहीं होता, मानो यह एक अधूरे प्रकाश में या अंधकार में अपने सच्चे धर्म की खोज कर रहा हो, और आत्म-उपलब्धि एवं पूर्णता तक पहुँचने से पहले यह अपने पथ पर अनेक निम्नतर और मिथ्या रूपों, अंतहीन त्रुटियों, विकृतियों, आत्म-हानियों, आत्म-प्राप्तियों, आदर्श और नियम की खोजों से गुजरता है। हमारी प्रकृति यहाँ ज्ञान और अज्ञान, सत्य और मिथ्या, सफलता और विफलता, सही और गलत, प्राप्ति और हानि, पाप और पुण्य का एक मिश्रित ताना-बाना है। सदा यह स्वभाव ही होता है जो इन सभी चीजों में से आत्म-अभिव्यक्ति और आत्म-उपलब्धि की खोज करता रहता है, 'स्वभावस्तु प्रवर्तते', यह एक ऐसा सत्य है जिससे हमें सार्वभौम उदारता और समदर्शिता का पाठ सीखना चाहिए, क्योंकि हम सभी इस एक ही कठिनाई और संघर्ष में ग्रस्त हैं। ये क्रियाएँ जीव की नहीं अपितु प्रकृति की हैं। पुरुषोत्तम इस अज्ञान से सीमित नहीं हैं; वे ऊपर से इसका संचालन करते हैं और जीव को उसके परिवर्तनों में से मार्ग दिखाते हैं। शुद्ध निर्विकार आत्म-सत्ता को ये क्रियाएँ छू तक नहीं पातीं; वह अपनी अगोचर-अस्पृश्य शाश्वत स्थिति के द्वारा इस क्षर प्रकृति को इसके उतार-चढ़ावों में साक्षी-भाव से देखती और आश्रय देती है। व्यक्ति की वास्तविक आत्मा, हमारे अंदर की केंद्रीय सत्ता, इन चीजों से महत्तर है, फिर भी प्रकृति के अंदर अपने बाह्य क्रमविकास में वह इन्हें अंगीकार करती है। और जब हम इस वास्तविक आत्मा, हमें धारण करनेवाली अपरिवर्तनशील विश्वगत आत्मा, प्रकृति के संपूर्ण व्यापार की अध्यक्षता करने वाले और परिचालन करनेवाले अपने अंतरस्थ पुरुषोत्तम या परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन के धर्म के समस्त आध्यात्मिक मर्म का पता पा लेते हैं। क्योंकि तब हम उन जगदीश्वर के विषय में सज्ञान हो जाते हैं जो अपने अनंत गुणों में, सर्व भूतों में अपने को सदैव प्रकट करते रहते हैं। हम भगवान् की चतुर्विध उपस्थिति के विषय में सज्ञान हो जाते हैं, वह है आत्म-ज्ञान और विश्व-ज्ञान की सत्ता, बल और शक्ति की सत्ता जो अपनी शक्तियों की खोज करती, उन्हें प्राप्त करती और प्रयोग में लाती है, पारस्परिकता एवं सृष्टि की तथा जीव-जीव के बीच संबंध एवं आदान-प्रदान की सत्ता, कर्म की सत्ता जो विश्व में श्रम करती है और प्रत्येक में सबकी सेवा करती है और प्रत्येक के श्रम को अन्य सबको सेवा में प्रयुक्त करती है। हम अपने अंदर भगवान् की जो व्यष्टि-शक्ति विद्यमान है उसके प्रति भी सचेतन हो उठते हैं, यह वह शक्ति है जो इन चतुर्विध शक्तियों को सीधे ही प्रयोग में लाती है, आत्म-अभिव्यक्ति के हमारे प्रयास को नियत करती है, हमारे दिव्य कर्म और पद का निर्धारण करती है और इस सबके द्वारा वह हमें बहुविधता में भगवान् के विश्वात्मभाव की ओर उठा से सलती है जब तक कि हम इसके द्वारा उनके साथ तथा इस सृष्टि में वेची कुछ हैं उस सबके साथ अपना आध्यात्मिक एकत्व प्राप्त नहीं कर लेते।
हमारी निम्न प्रकृति को हमारे स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण वह अनेकानेक प्रकार के उतार-चढ़ावों से गुजरती है। इसीलिए हमारी त्रिगुणमय निम्न प्रकृति में त्रुटियाँ, विकृतियाँ, सत्य-असत्य आदि सभी एक-दूसरे से मिले-जुले रहते हैं जिनमें मनुष्य भ्रमित होकर भटकता रहता है, ठोकरें खाता रहता है। हालाँकि जीव को भीतर से अपने सच्चे स्वभाव का पता होता है परंतु सतही प्रकृति में उसके विषय में अनभिज्ञ होने के कारण उसे इन सभी उतार-चढ़ावों और थपेड़ों से गुजरना पड़ता है। और धीरे-धीरे ही व्यक्ति को अपनी सच्ची प्रकृति का या फिर अपने स्वभाव का पता लगता है। अतः हमें सफलता-असफलता, हर्ष-शोक, लाभ-हानि आदि सभी द्वंद्वों से गुजरना होता है परंतु हमारी आंतरिक प्रकृति हमारी बाह्य प्रकृति के इन क्रियाकलापों से अक्षुब्ध रहती है और इसे साक्षी भाव से देखती है। परंतु चूँकि यह बाह्य या निम्न प्रकृति पराप्रकृति की ही अभिव्यक्ति का क्षेत्र है अतः वह निम्न प्रकृति और उसके क्रियाकलापों से महत्तर होते हुए भी इसकी क्रिया को स्वयं अपनाती है। और वास्तव में यदि हमारी निम्न प्रकृति की क्रियाओं को हमारी आंतरिक प्रकृति का अवलंबन प्राप्त न हो तो वह चल ही नहीं सकती। अतः इसी प्रतीयमान निम्न कार्य-व्यापार में से भी आंतरिक प्रकृति हमारी बाहरी प्रकृति को हमारे अंतरस्थ परमेश्वर की ओर निर्देशित करती है और जब हम उस अंतरस्थ उपस्थिति के विषय में सज्ञान हो जाते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं तब अपने जीवन के आध्यात्मिक मर्म को जान जाते हैं और साथ ही हम इस बारे में भी सज्ञान हो जाते हैं कि किस प्रकार भगवान् चतुर्विध रूप से सभी भूतों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और इन चारों को श्रीअरविन्द ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकट किया है। इससे अब पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार जिन्हें हम चतुर्वर्ण कहते हैं वह तो भगवान् का चतुर्विध रूप है जिसका वास्तव में अभिप्राय किसी बाह्य क्रिया से नहीं अपितु भगवान् के चार भावों से है। साथ ही व्यक्ति इस विषय में भी सचेत हो जाता है कि उसके अंदर भगवान् की चतुर्विध शक्तियों में से कौनसी शक्ति अधिक क्रियारत है और वह यह भी जान जाता है कि वही विशिष्ट शक्ति, जिसे स्वभाव कहते हैं, उसके सारे बाह्य कर्मों आदि को नियत करती है। परंतु वह केवल व्यष्टिभाव तक ही नहीं रुकती अपितु बहुविधता में भगवान् के विश्वात्मभाव की ओर उठा ले चलती है अर्थात् भगवान् की अन्य शक्तियों को भी विकसित करती है जब तक कि हम इस सृष्टि में भगवान् जो कुछ भी हैं उस सबके साथ अपना आध्यात्मिक एकत्व प्राप्त नहीं कर लेते। अतः अंतरतम रूप से तो व्यक्ति स्वयं परमात्मा ही है इसलिए उसकी क्रिया में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हो सकता, केवल बाह्यतर क्रिया में ही चतुर्वर्ण का विचार आता है। इसी को श्रीअरविन्द बता रहे हैं।
जीवन में मनुष्यों के चतुर्वर्ण का बाह्य विचार दिव्य क्रिया के इस सत्य की बाह्यतर क्रिया से ही सम्बन्ध रखता है; वह त्रिगुण के कार्य-व्यापार में इसकी क्रिया के एक पहलू तक ही सीमित है। यह सच है कि इस जन्म में मनुष्य अधिकतर चार श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत होते हैं - ज्ञानी मनुष्य, बलशाली मनुष्य, उत्पादनशील प्राणिक मनुष्य और स्थूल श्रम एवं सेवा में परायण मनुष्य। ये आधारभूत विभाग नहीं हैं अपितु हमारे मनुष्यत्व में आत्म-विकास की अवस्थाएँ हैं। मनुष्य अज्ञान और जड़ता के पर्याप्त बोझ के साथ शुरू करता है; उसकी पहली अवस्था उस स्थूल श्रम की होती है जो शरीर की आवश्यकताओं, प्राण की प्रेरणा एवं विश्वप्रकृति के अलंघ्य नियम के द्वारा और, आवश्यकता की किसी सीमा के परे, समाज के द्वारा उस पर थोपी गयी किसी-न-किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष बाध्यता के द्वारा उसके पाशविक तमस् पर लादा जाता है, और जो लोग अभी भी इस तमस् के द्वारा शासित होते हैं वे शूद्र होते हैं, समाज के दास होते हैं जो उसे अपना श्रम दान करते हैं तथा उसके जीवन की बहुविध क्रीड़ा में वे अधिक उन्नत मनुष्यों की तुलना में और कुछ भी योगदान नहीं कर सकते अथवा यदि कर भी सकते हैं तो बहुत ही कम। कार्य-प्रवृत्ति या गतिशील कर्म के द्वारा मनुष्य अपने अन्दर राजसिक गुण का विकास करता है और हमें एक दूसरी श्रेणी का मनुष्य प्राप्त होता है जो उपयोगी सृजन, उत्पादन, संग्रह, उपार्जन, अधिकार और उपभोग की सतत् प्रेरणा से चालित होता है, वह मध्यवर्गीय आर्थिक और प्राण-प्रधान मनुष्य, वैश्य, होता है। हमारी एक समान ही सार्वभौम प्रकृति के राजसिक या प्रवृत्तिमय गुण का उच्चतर उत्कर्ष होने पर एक क्रियाशील मानव हमारे देखने में आता है जिसमें एक प्रबलतर संकल्पशक्ति एवं अधिक साहसपूर्ण महत्त्वाकांक्षाएँ होती हैं, कर्म करने, युद्ध करने, अपने संकल्प को क्रियान्वित करने और, अपने सबलतम रूप में, नेतृत्व करने, आदेश देने, शासन करने, जन-समुदायों को अपने पथ पर चलाने की एक सहज प्रवृत्ति होती है, वह राजा, क्षत्रिय होता है। और जहाँ याधान होता है वहाँ हमें ब्राह्मण की प्राप्ति होती है, जिसकी प्रवृत्ति ज्ञान की प्रधान होती है, जो जीवन के अंदर विचार, चिंतन, सत्य की खोज और एक ज्ञानपूर्ण या उच्चतम स्थिति में एक आध्यात्मिक शासन ले आता है और उसके द्वारा वह अपनी जीवन की धारणा और उसकी शैली को आलोकित करता है।
बाहरी रूप से मनुष्य भले कोई भी वर्ण का क्यों न हो तो भी सामान्य क्रम में हम देखते हैं कि उस पर तमस् का प्रभाव अधिक रहता है। मनुष्य के जीवन काल में हम प्रारंभिक समय में देख सकते हैं कि सामान्यतः बालक, यदि वह अतिविशिष्ट हो तब तो अलग बात है, अज्ञान में होता है जिसकी क्रियाएँ पाशविक प्रकार की होती हैं। ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। ज्यों-ज्यों चेतना में विकास होता है तब व्यक्ति केवल अपने ही ऊपर केंद्रित न रहकर दूसरों की सत्ता को स्वीकार करता है और समाज में रहने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए वस्तुओं, व्यक्तियों, पशु-पक्षियों आदि सभी के साथ आवश्यक आदान- प्रदान के नियम को, उनके बीच तालमेल के विधान को समझने लगता है। इस प्रकार यह तामसिक चेतना से राजसिक में आरोहण होता है। इसी तालमेल, उपार्जन, संचय आदि की प्रवृत्ति को वैश्य की संज्ञा दी गई है। इसी राजसिक प्रवृत्ति का जब विकास होता है तब हमें उच्चतर प्राणिक क्रियाएँ देखने को मिलती हैं जिसमें व्यक्ति साहसिक और प्रबल संकल्पशक्ति के कार्य और अभियान कर सकता है। इसी उच्चतर प्राण प्रधान प्रवृत्ति को क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है। और जब इससे अधिक विकसित होकर व्यक्ति में मनःतत्त्व का विकास होता है तब इसके प्रभाव से वह उचित-अनुचित, सत्य-असत्य आदि का विचार करता है और तब इस सात्त्विक प्रवृत्ति को ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। यह श्रेणीकरण या विभाजन की पद्धति सर्वथा गुणात्मक है जिसका कि केवल आंतरिक और मनोवैज्ञानिक आधार होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सारा चेतना का एक क्रमविकास है और इसी संबंध में हमारी संस्कृति में यह प्रचलित था कि जन्म से सभी शूद्र ही पैदा होते हैं। अतः यह तर्कसम्मत हो है कि किसी शूद्र चेतना को किन्हीं गंभीर सत्यों के प्रति उद्घाटित करने के लिए पहले विकास के क्रम से गुजरना होगा अन्यथा वह उन सत्यों का दुरुपयोग करके स्वयं अपने आप को तथा दूसरों को संकट की स्थिति में डाल सकती है। इसी अर्थ में यह उक्ति कि 'जन्मना जायते शूद्र' आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि वह अपने प्राकट्य के समय थी।* हमारे सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी को कोई गंभीर बात बताने में या किसी के साथ कोई व्यवहार करने में हम अधिकारी-अनधिकारी भेद पर सदा ही विचार करते हैं।
जब हम चेतना के इस क्रमविकास के अनुसार मनुष्यों के विषय में विचार करते हैं तब अधिकांश मनुष्यजाति तो पहले या दूसरे विभाजन तक ही ठहर जाती है। पहले और दूसरे की तुलना में तीसरे विभाग में हमें बहुत ही अल्प संख्या में लोग देखने को मिलते हैं और चौथे विभाग में तो उससे भी बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलते हैं जो कि वास्तव में ब्राह्मण हों। जब व्यक्ति बिल्कुल पाशविक चेतना के ही निकट होता है तब उसके कर्मों का उत्प्रेरण भय या फिर कामना के द्वारा ही होता है। यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो अधिकांशतः तो मनुष्य इसी लिए कर्म करते दिखाई देते हैं क्योंकि यदि वे ऐसा न करें तो उनका स्वयं का तथा उनके परिवार का भरण-पोषण नहीं होगा या फिर इसलिए क्योंकि वे कर्म न करने के सहज परिणामों से भयभीत होते हैं। ऐसे लोग तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि कर्म के व्यक्तिगत परिणाम क्या होंगे या जो किसी आदर्श की सिद्धि के लिए, किसी उचित-अनुचित के बोध से चालित होकर कर्म करते हैं।
-------------------------------
* वैदिक ऋषियों का प्रतीकों के प्रयोगों में सदा ही केवल इसी बात पर ध्यान रहता था कि किस प्रकार सत्य का प्राकट्य अधिक से अधिक गहराई के साथ तथा मूर्तिमान रूप से हो सके। अतः उनके द्वारा 'जन्मना जायते शूद्र' की जो कहावत है उसमें चातुर्वर्ण्य में प्रयुक्त शूद्र शब्द का उपयोग कर लिया गया परंतु इस एक ही पद का दोनों ही स्थानों पर सर्वथा भिन्न-भिन्न अर्थ है। संकुचित दृष्टिकोण अपनाने पर बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है जिस कारण इस उक्ति को कि 'शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है' वर्ण-व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है जो कि समाज में भारी भेदभाव व दुर्भावना पैदा कर देता है जबकि यदि इसे 'जन्मना जायते शूद्र' से जोड़ा जाये तो इससे कोई विषमता पैदा नहीं की जा सकती क्योंकि इसका सत्य तो सभी के लिए सदा ही स्पष्ट रूप से प्रकट है।
सभी को इस चेतना के क्रमविकास की अवस्थाओं से गुजरना होता है। यदि पूर्वजन्म में किसी ने बहुत विकास साधित कर लिया हो वह आगामी जन्मों में शीघ्र ही उतनी अवस्था को प्राप्त कर लेगा परंतु चाहे कितना ही शीघ्र क्यों न हो तो भी उसे उस विकासक्रम से जाना ही होता है। अतः अपने जीवन के आरंभिक काल में व्यक्ति शूद्र होता है और उस अवस्था से गुजरकर वह आगे का आरोहण करता है। परंतु इसका गीता की वर्ण-व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। हमारी आन्तरिक सत्ता में हम सभी द्विज हैं और बाह्य स्थूल भौतिक सत्ता में शूद्र हैं। जितनी ही अधिक हमारी आंतरिक सत्ता विकसित होगी हमारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी और बाह्य सत्ता पर उतना ही अधिक वह अपना दबाव डालकर उसे सुसंस्कृत बना सकती है। और एक सीमा के बाद जब आत्मा इतनी पर्याप्त रूप से प्रबल हो जाती है तब वह मुक्त रूप से सत्ता के अन्य भागों को अपने उपकरण के रूप में प्रयोग करती है और तब उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रहती। तब व्यक्ति कर्तव्यं कर्म के रूप में कर्म करता है न कि किसी प्रकार के भय या कामना के कारण। यह एक सर्वथा भिन्न मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसको बाहरी कर्मों से बहुत अधिक परखा नहीं जा सकता। बाहरी कर्म समान भी हों तो भी मनोवैज्ञानिक स्थिति सर्वथा भिन्न हो सकती है।
मानव-प्रकृति में इन चारों व्यक्तित्वों का कुछ-न-कुछ अंश सदा हो होता है, चाहे वह विकसित हो या अविकसित, व्यापक हो या संकुचित, दबा हुआ हो या ऊपरी सतह की ओर उठ रहा हो, परन्तु अधिकांश मनुष्यों में प्रायः इनमें से कोई एक या दूसरा प्रबल होता है और कभी-कभी तो वह प्रकृति में कर्म के सम्पूर्ण क्षेत्र को हस्तगत करता प्रतीत होता है। और किसी भी समाज में चारों ही श्रेणियाँ होनी चाहिए, - भले ही, उदाहरण के लिए, हम एक ऐसा निरा उत्पादनशील और व्यावसायिक समाज क्यों न बना सकते हों जिसके लिए आधुनिक युग ने प्रयत्न किया है, या उसी प्रयोजन के लिए श्रमिकों का, निम्नतम श्रेणी के लोगों का एक ऐसा शूद्र-समाज क्यों न बना सकते हों जैसा कि अत्यंत आधुनिक मन को आकृष्ट करता है और जिसे आज यूरोप के एक भाग में आजमाया जा रहा है तथा अन्य भागों में समर्थन किया जा रहा है। फिर भी कुछ ऐसे विचारक तो रहेंगे हो जो सम्पूर्ण विषय का के कुछ ऐसे अध्यक्ष और नायक भी रहेंगे जो इस समस्त उत्पादक कर्म के विधान, सत्य और मार्गदर्शक नियम ढूँढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, उद्योग-व्यवान बहाने साहस, युद्ध, नेतृत्व और प्रभुत्व की अपनी माँग को तृस करेंगे, बहत से विशिष्ट निरे उत्पादनशील और धनोपार्जक मनुष्य तथा कुछ ऐसे औसत मजदूर भी रहेंगे ही जो थोड़े से श्रम और उसके पुरस्कार से संतुष्ट होंगे। परन्तु ये सर्वथा बाह्य चीजें हैं, और यदि यही सब कुछ हो तो, मानवजाति की इस श्रेणी-व्यवस्था का कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं होगा। अथवा, जैसा कि कभी भारतवर्ष में माना जाता था, इसका अर्थ अधिक-से-अधिक यह होगा कि हमें अपने जन्मों में विकास की इन अवस्थाओं में से गुजरना होगा; क्योंकि हमें बाध्य होकर तामसिक, राजस-तामसिक, राजसिक या राजस-सात्त्विक प्रकृति से उत्तरोत्तर सात्त्विक प्रकृति की ओर अग्रसर होना होगा, एक आंतरिक ब्राह्मणत्व, 'ब्राह्मण्य' की ओर आरोहण करना और उसी में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित होना होगा और फिर उस आधार से मोक्ष के लिए यत्न करना होगा। परन्तु ऐसी दशा में, गीता के इस कथन के लिए कोई युक्तिसंगत स्थान नहीं रहेगा कि शूद्र या चांडाल भी अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़कर सीधे आध्यात्मिक स्वातंत्र्य और पूर्णत्व की ओर आरोहण कर सकता है।
मूलभूत सत्य यह बाह्य वस्तु नहीं है, अपितु हमारी गतिशील अंतः-सत्ता ५ की एक शक्ति है, आध्यात्मिक प्रकृति की चतुर्विध सक्रिय शक्ति का सत्य है। अपनी आध्यात्मिक प्रकृति में जीव के ये चार पक्ष होते हैं - वह एक ज्ञान की सत्ता, बल की और शक्ति की सत्ता, परस्परभावसंपन्न तथा आदान-प्रदानात्मक सत्ता और कर्ममय एवं सेवात्मक सत्ता होता है, परन्तु कर्म में तथा अभिव्यक्तिकारक भाव में कोई एक या दूसरा पक्ष प्रधान होता है और वह देहधारी प्रकृति के साथ जीवन के व्यवहारों को अपना पुट दे देता है; वह अन्य शक्तियों का नेतृत्व करता तथा उन पर अपनी छाप लगा देता है और कर्म, प्रवृत्ति और अनुभूति की प्रधान धारा या झुकाव के निमित्त उनका प्रयोग करता है। तब स्वभाव सामाजिक वर्ण-विभाग में प्रतिपादित कर्त्तव्य-भेद के अनुसार स्थूल और कठोर रूप में नहीं अपितु सूक्ष्म और सहजनम्य रूप में इस धारा के धर्म का अनुसरण करता है और इसका विकास करते हुए अन्य तीन शक्तियों का भी विकास करता है।
-----------------------------
* प्राचीनों का यह मानना था कि सभी मनुष्य अपनी निम्नतर प्रकृति में शूद्रों के रूप में उत्पन्न होते हैं और नैतिक तथा आध्यात्मिक संस्कार के द्वारा ही द्विज बनते हैं, पर अपनी उच्चतम आन्तरिक सत्ता में सभी ब्राह्मण होते हैं जो पूर्ण आत्मस्वरूप एवं देवत्व प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो कदाचित् हमारी प्रकृति के मनोवैज्ञानिक सत्य से दूर नहीं है।
इस प्रकार कर्म और सेवा की सहज-वृत्ति का ठीक ढंग से अनुसरण ज्ञान को विकसित करता, शक्ति वर्द्धित करता है, पारस्परिक घनिष्ठता या संतुलन तथा सम्बन्ध की कुशलता एवं सुश्रृंखला को साधता है। चतुर्विध देवत्व का प्रत्येक प्रश्न अपने प्रधान स्वभावाम तत्त्व के विस्तार और अन्य तीनों के द्वारा समृद्ध होकर अपनी समग्र पूर्णता की और गति करता है। यह प्रगति त्रिगुण के नियम के अनुसार होती है। ज्ञानमय सत्ता के धर्म का अनुसरण करने का एक तामसिक और राजसिका ढंग भी हो सकता है, शक्ति के धर्म का अनुसरण करने का एक क्रूर तामसिका तथा उच्च सात्विक ढंग भी हो सकता है, कर्म और सेवा के धर्म के पालन का एक शक्तिपूर्ण राजसिक या सुन्दर एवं उदात्त सात्त्विक ढंग भी हो सकता है। आंतरिक व्यक्तिगत स्वधर्म के तथा जीवन-पथ पर वह हमें जिन कर्मों की ओर ले जाता है उनके सात्त्विक रूप तक पहुँचना पूर्णता प्राप्त करने की प्राथमिक शर्त है। और यह ध्यान देने योग्य है कि आंतरिक स्वधर्म कर्म, पेशे या कर्त्तव्य के किसी बाह्य सामाजिक या अन्य रूप से नहीं बँधा होता। उदाहरणार्थ, हमारी कर्ममय सत्ता जो सेवा करने से ही तृप्त होती है या हमारे अन्दर का यह कर्ममय तत्त्व ज्ञानान्वेषण के जीवन, संघर्ष-प्रधान और शक्तिमय जीवन या पारस्परिक सम्बन्ध, उत्पादन और आदान-प्रदान के जीवन को अपनी श्रम और सेवा की दिव्य प्रेरणा की तृप्ति का साधन बना सकता है।
अतः गीता का विधान यह है कि भले बाहरी रूप से व्यक्ति जिस किसी भी वर्ण में क्यों न हो परंतु जो भी उसका आंतरिक भाव होगा उसी के अनुसार गति करते-करते उसमें अन्य भाव भी विकसित होंगे और व्यक्ति इन सभी के साथ मद्भाव में जा सकेगा। उदाहरण के लिए बाहरी रूप से व्यक्ति वैश्य के आदान-प्रदान का कार्य कर रहा हो परंतु आंतरिक सत्ता में उसमें गहरा सेवा भाव हो तो वह उसी भाव को विकसित करता है।
____________________
*व्यक्तित्व के इन चार भेदों में से कोई भी यदि अन्य गुणों का कुछ अंश अपने अन्दर नहीं लाता तो वह अपने क्षेत्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, ज्ञानी मनुष्य स्वतंत्रता और पूर्णता के साथ सत्य की सेवा नहीं कर सकता यदि उसमें बौद्धिक और नैतिक साहस, संकल्प एवं निर्भयता, तथा नये राज्यों के द्वार खोलने एवं उन्हें जीतने की सामर्थ्य न हो, अन्यथा वह सीमित बुद्धि का दास बन जाता है अथवा केवल किसी प्रतिष्ठित ज्ञान का एक सेवक या, अधिक-से-अधिक उसका एक कर्मकाण्डीय पुरोहित बनकर रह जाता है - अपने ज्ञान को सर्वोत्तम लाभ के लिये प्रयोग में नहीं ला सकता जब तक कि उसके सत्यों को जीवन के व्यवहारार्थ क्रियान्वित करने के लिये उसके अन्दर अनुकूलनशील कौशल न हो, अन्यथा वह केवल विचार में ही निवास करता रहता है, अपने ज्ञान का पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर मानव जाति के प्रति, मनुष्य में अवस्थित भगवान् तथा अपनी सत्ता के स्वामी के प्रति सेवा का भाव न हो। (इसी प्रकार) शक्तिप्रधान मनुष्य (क्षत्रिय) को अवश्य ही अपनी शक्ति, अपने बल को ज्ञान के द्वारा, बुद्धि या धर्म या आत्मा के प्रकाश के द्वारा आलोकित, उन्नत और संचालित करना चाहिए, अन्यथा वह महज शक्तिशाली असुर बन जायेगा, - उसके अन्दर वह कौशल होना चाहिये जो उसे अपनी शक्ति को प्रयुक्त, परिचालित एवं नियमबद्ध करने एवं सर्जनशील और फलप्रद रूप देने में तथा दूसरों के साथ उसके सम्बन्धों के लिये उपयुक्त बनाने में सर्वोत्तम सहायता करे, अन्यथा वह जीवन के क्षेत्र के आर-पार शक्ति का एक प्रचण्ड प्रवाह, एक ऐसे तूफान का रूप ले लेती है जो प्रबल वेग से आता है और रचना करने की अपेक्षा कहाँ अधिक विनाश करके चला जाता है, - साथ ही वह (क्षत्रिय) आज्ञापालन करने में भी समर्थ होना चाहिये और अपनी शक्ति का प्रयोग ईश्वर और जगत् की सेवा के लिये करना । चाहिये, अन्यथा वह एक स्वार्थी शासक, अत्याचारी तथा मनुष्यों की आत्माओं और शरीरों का क्रूर दमनकारी बन जाता है। उत्पादनशील मनोवृत्ति और कार्यप्रवृत्ति रखने वाले मनुष्य में खुला जिज्ञासाशील मन, उर्वर विचार और ज्ञान होना चाहिये, अन्यथा वह विस्तारशील विकास के बिना अपने दैनिक कार्य-व्यापार के सीमित घेरे में ही विचरण करता रहता है, उसमें साहस और बड़े कार्य का बीड़ा उठाने की वृत्ति भी होनी चाहिये, अपने उपार्जन और उत्पादन के कार्य में सेवा की भावना लानी चाहिये, ताकि वह केवल उपार्जन ही न करे, अपितु दान भी कर सके, केवल बटोर करके अपने जीवन के सुखों का ही उपभोग न करे, अपितु अपने चारों ओर के जीवन की, जिससे वह लाभ उठाता है, फलशालिता और पूर्ण समृद्धि में सचेतन रूप से सहायता पहुँचाये। (इसी प्रकार) यदि श्रम और सेवा करने वाला व्यक्ति (शूद्र) अपने कार्य में ज्ञान, सम्मान-भावना, अभीप्सा और दक्षता न लाये तो वह एक असहाय श्रमिक एवं समाज का दास बन जाता है, क्योंकि उक्त गुणों को अपने अन्दर लाकर ही वह ऊर्ध्वान्मुख मन और संकल्पशक्ति तथा सद्भावनापूर्ण उपयोगिता के द्वारा उच्चतर वर्णों के धर्मों की ओर उठ सकता है। परन्तु मनुष्य की महत्तर पूर्णता तभी साधित होती है जब वह अपने-आप को विशाल बनाकर इन चारों शक्तियों को अपने अन्दर समाविष्ट कर लेता है और अपनी प्रकृति को चतुर्विध आत्मा की सर्वतोमुखी पूर्णता एवं विराट् शक्ति-सामर्थ्य की ओर अधिकाधिक खोलता जाता है, यद्यपि इन चारों में से कोई एक अन्यों का नेतृत्व भी कर सकती है। मनुष्य इन धर्मों में से किसी एक की एकांगी प्रकृति के रूप में गढ़ा हुआ नहीं है, अपितु आरम्भ में उसके अन्दर ये सभी शक्तियाँ अनगढ़ एवं अव्यवस्थित रूप में कार्य कर रही होती हैं, पर उत्तरोत्तर जन्मों में वह किसी एक या दूसरी शक्ति को रूप प्रदान करता है, एक ही जीवन में किसी एक से दूसरी की ओर प्रगति करके अपने आंतरिक अस्तित्व के समग्र विकास की ओर बढ़ता जाता है।
उस सेवा भाव में ही कोई प्रसंग ऐसा भी उठ खड़ा हो सकता है कि व्यक्ति को किसी की रक्षा करने के लिए क्षात्र तेज भी विकसित करना हो। सेवा करने के क्रम में ही व्यक्ति को कोई साहसिक कार्य करने की भी आवश्यकता हो सकती है और उसी के द्वारा उसमें वह भाव भी विकसित हो सकता है। साथ ही, सच्ची सेवा करने के लिए सच्चा ज्ञान भी होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के हम सच्ची सेवा नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी एक ही भाव से आरंभ करके व्यक्ति धीरे-धीरे अन्य भावों को भी विकसित करता है। लक्ष्मण जी के उदाहरण से हमें यही देखने को मिलता है। जब उन्हें राजकार्य के लिए कहा गया तब उन्होंने यह कहते हुए उससे इन्कार कर दिया कि उनका धर्म तो सेवा-धर्म है। अब बाहरी वर्ण के अनुसार तो लक्ष्मण जी और भरत जी क्षत्रिय ही थे, परंतु उनका भीतरी भाव सेवा का था और उसी भाव के द्वारा उन्होंने अपने अन्य भावों को भी विकसित किया। श्रीरामचरितमानस में हम देखते हैं कि बाहरी रूप से परम् शूरवीर, बलशाली योद्धा होते हुए भी उनका आंतरिक भाव श्रीराम के सेवक का था। अतः गीता का यही विधान है कि जो आंतरिक चतुर्विध ब्रह्म है वह किसी भी भाव से आरंभ कर के अन्य भावों को भी इस शरीर में विकसित करेगा।
और अन्त में, इस चतुर्विध कर्म के दिव्यतम रूप और इसकी अत्यंत क्रियाशील आत्म-शक्ति को प्राप्त करना सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की तीव्रतम और व्यापकतम यथार्थता का बृहत् द्वार है। ऐसा हम तभी कर सकते हैं यदि हम स्वधर्म की क्रिया को अन्तर्वासी देव, विश्वगत परमात्मा और परात्पर पुरुषोत्तम की पूजा में परिणत कर दें और, अन्ततः, सम्पूर्ण कर्म उनके हाथों में समर्पित कर दें, 'मयि संन्यस्य कर्माणि'। तब जिस प्रकार हम तीन गुणों के सीमाबंधन से परे चले जाते हैं उसी प्रकार हम चातुर्वर्ण्य-विभाग से तथा सभी विशिष्ट धर्मों की सीमा से भी परे चले जाते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य। विश्व-पुरुष व्यक्ति को विश्वगत स्वभाव में उठा ले जाता है, हमारे अन्दर की चतुर्विध प्राकृत सत्ता को पूर्ण बनाता और एक करता है और जीव के अन्दर विराजमान परमेश्वर के दिव्य संकल्प तथा उपलब्ध की गई शक्ति के अनुसार अपने आत्म-निर्धारित कर्मों को संपन्न करता है।
परमेश्वर के दिव्य संकल्प तथा उपलब्ध की गई शक्ति के अनुसार अपने आत्म-निर्धारित कर्मों को संपन्न करना ही गीता का सच्चा अर्थ हो सकता है क्योंकि इसके तुरंत बाद ही गीता परम् रहस्य की ओर अग्रसर होती है। गीता किसी कर्मकाण्ड और किसी सामाजिक व्यवस्था की शिक्षा नहीं देती अपितु व्यक्ति के अंदर विराजमान भगवान् की चतुर्विध सत्ता को विकसित करके उससे भी परे ले जाती है। गीता की वास्तविक शिक्षा अब आरंभ होगी जिसे ही प्रदान करने के लिए शेष सब तो केवल तैयारी मात्र या भूमिका स्वरूप ही थीं।
प्रश्न : श्रीअरविन्द कहते हैं कि इन चारों वर्णों में से एक को आधार बनाकर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो शेष तीनों वर्ण उसका समर्थन कर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसका क्या अर्थ है?
उत्तर : ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान् के चारों ही गुण अविभाज्य रूप से परस्पर संबद्ध हैं। जैसे किसी व्यक्ति के दोनों हाथ किसी एक ही देह के अविभाज्य अंग हैं और देह के गति करने पर दोनों ही हाथ साथ-साथ ही गति करेंगे उसी प्रकार ये चारों ही भगवान् की देह के चतुर्विध पहलू हैं जिन्हें भिन्न-भिन्न नहीं किया जा सकता। अतः मूलतः तो चारों ही वर्ण साथ-साथ होते हैं इसलिए चारों को पूर्ण किये बिना कोई भी एक अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। ये तो श्रीमाताजी की चार शक्तियों की तरह हैं तथा जो श्रीमाताजी की अनन्त शक्तियों में से ऐसी हैं जो धरती पर प्रमुख रूप से क्रियारत हैं जिनके द्वारा वे अभिव्यक्त हो रही हैं। इन महान् शक्तियों को, जिनके नाम क्रमशः महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्णों की अधिष्ठात्री देवियों के रूप में जान सकते हैं। अतः किसी एक भी शक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे सभी जगज्जननी के एक अखण्ड रूप की ही अभिन्न अंग हैं और किसी एक को भी छोड़ देने पर तो वह स्वरूप अखण्ड नहीं रह सकता। इस कारण, बाहरी रूप से व्यक्ति के जो भी क्रियाकलाप क्यों न हों, परंतु आंतरिक रूप से चारों ही शक्तियाँ साथ-साथ गति करती रहती हैं। गीता का यह एक ऐसा विलक्षण तत्त्व है जिसे केवल श्रीअरविन्द ही प्रकट करते हैं।
III. परम् रहस्य की ओर
श्रीगुरु और जो कुछ भी कहना चाहते थे वह सब वे कह चुके हैं, वे अपने संदेश के सभी प्रधान तत्त्वों, सहायक निर्देशों और निहित अर्थों का निरूपण कर चुके हैं, उसके विषय में जो मुख्य संशय और प्रश्न उठ सकते हैं उन्हें स्पष्ट कर चुके हैं, और अब उनके लिए प्रकट करने के लिए जो कुछ शेष रह जाता है वह है अपनी अंतिम वाणी, अपने संदेश का मर्म, अपनी शिक्षा के सारतत्त्व मात्र को निर्णायक शब्दों और हृदयस्पर्शी सूत्र में प्रकट करना। और हम पाते हैं कि वह निर्णायक अंतिम और परम वचन, इस विषय पर पहले जो कुछ भी कहा जा चुका है केवल उसका सार मात्र ही नहीं है, अभीष्ट साधना का और इसके समस्त तप और पुरुषार्थ के परिणामस्वरूप प्राप्त होनेवाली महत्तर अध्यात्म-चेतना का केवल घनीभूत वर्णन मात्र ही नहीं है वह तो मानो वेगवान् रूप से और अधिक आगे की ओर उड़ा ले जाता है. बहधक्क सीमा तथा नियम-मर्यादा और विधि-विधान को तोड़ डालता है और अनंत अर्थ से गर्भित एक विशाल एवं असीम आध्यात्मिक सत्य का इए खोल देता है। और वह गीता की शिक्षा की गंभीरता एवं व्यापक विस्तार का तथा उसके भाव की महत्ता का एक चिह्न है। एक साधारण धार्मिक शिक्षा या दार्शनिक सिद्धान्त सत्य के किन्हीं महत् और प्राणवंत पहलुओं को अधिकृत करके तथा उन्हें मनुष्य के अंतर्जीवन का और उसके कर्म के विधान और स्वरूप का मार्गदर्शन करने के लिए एक उपयोगी मत-वाद, उपदेश, पद्धति एवं साधना का रूप देकर ही भली-भाँति संतुष्ट हो जाता है; वह इससे आगे
नहीं जाता, वह अपनी पद्धति के घेरे के बाहर निकलने के लिए द्वार नहीं खोलता, उससे बाहर निकालकर हमें किसी विस्तीर्णतम स्वतंत्रता और बंधनमुक्त विशालता में नहीं ले जाता। यह सीमाबंधन उपयोगी है और निश्चया ही कुछ समय के लिए अनिवार्य भी है। अपने मन और संकल्प के द्वारा परिसीमित मनुष्य को अपने विचार और कर्म के संबंध में एक नियम और विधान की, एक नियत-निर्धारित पद्धति की और एक सुनिश्चित अभ्यासक्रम की आवश्यकता होती है; वह माँग करता है उस एक ही अचूक और कटे-छँटे मार्ग की, जो बाड़ किया हुआ एवं सुनिर्दिष्ट हो और जिस पर पैर रखना सुरक्षित हो, वह चाहता है सीमित क्षितिज, समावृत पड़ाव । केवल बलवान् और विरले ही व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। और फिर भी जिन रूपों और प्रणालियों में मन संतुष्ट रहता है और अपना सीमित सुख लाभ करता है उनसे अंततः बाहर निकलने का कोई मार्ग मुक्त जीव के लिए होना ही चाहिए। अपने आरोहण की सीढ़ी को पार कर जाना, उसके सबसे ऊपर के सोपान पर भी रुक न जाना अपितु अबाधित और व्यापक रूप से आत्मा की विशालता में विचरण करना एक ऐसी मुक्ति है जो हमारी पूर्णता के लिए आवश्यक है; आत्मा की परम स्वाधीनता ही हमारी सिद्ध अवस्था है। और गीता हमें इस ओर इस प्रकार ले जाती है: वह आरोहण के एक सुदृढ़ और निश्चित पर अत्यंत विस्तीर्ण मार्ग का, एक महान् धर्म का प्रतिपादन कर देती है, और फिर वह हमें जो कुछ प्रतिपादित किया जा चुका है उस सबसे बाहर निकालकर, उसके परे, सब धर्मों के परे अनंततः उन्मुक्त आकाशों में ले जाती है और एक पूर्ण आध्यात्मिक स्वाधीनता पर प्रतिष्ठित परम सिद्धि की आशा हमारे सामने प्रकट कर देती है, उसके रहस्य में हमारा प्रवेश करा देती है और वह 'गुह्यतमम्' रहस्य ही, उसके परम वचन का सार है, वही गूढ़ तत्त्व और अंतरतम ज्ञान है।
और सर्वप्रथम गीता अपने संदेश का स्वरूप पुनः प्रतिपादित करती है। वह उन पंद्रह श्लोकों की परिमित परिधि में संपूर्ण रूपरेखा और सारमर्म संक्षेप मैं वर्णित कर देती है, जिनकी पंक्तियों की भावाभिव्यंजना और अर्थ संक्षिप्त एवं घनीभूत है, जो मूल विषय के सार का कुछ भी बाकी नहीं छोड़ती जो कि अत्यंत विशद यथार्थता तथा सुबोधता से युक्त उक्तियों में व्यक्त किया गया है। और इसलिए इनका विश्लेषण बड़े ध्यान से करना होगा, जो कुछ पहले कहा जा चुका है उस सबके प्रकाश में गहराई के साथ इनका अध्ययन करना होगा, क्योंकि यहाँ स्पष्टतः अभिप्रेत है कि जिसे स्वयं गीता अपनी शिक्षा का केंद्रीय भाव समझती है उसका निहितार्थ प्रकाशित किया जाए।
परमात्मा तथा उनका परम् सत्य असीम है। परंतु मनुष्य जब अपने सीमित मन के द्वारा उसे जानने का प्रयास करते हैं तब वे उसे अपने मानसिक सूत्र के दायरे में बाँधने का प्रयास करते हैं। अपने स्वभाव मात्र में ही मन अखण्ड और समग्र रूप से उस परम् सत्य को देखने में असमर्थ है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही है किसी चीज को विभाजित करके प्रत्येक विभाजन का विश्लेषण करने की और उस विभाजन का विश्लेषण वह अपने सीमित इंद्रिय आधारित तरीके से करता है। इस कारण भले ही कितना भी विकसित मन क्यों न हो, फिर भी सत्य उसकी पकड़ से छूट निकलता है। हमारे ऋषियों के अनुसार भारतीय मन की यह विशेषता रही है कि वह अपने आप को निरपेक्ष सत्ता में प्रक्षिप्त करता है और बदले में उसे जो आभास प्राप्त होते हैं उनसे वह अपनी योग-प्रणालियों, धर्मों, तत्त्वदर्शनों आदि का निर्माण करता है। परंतु जैसे मानव चेतना से नीचे की चेतना अपनी ऊँची से ऊँची कल्पना के द्वारा भी मानव चेतना की थाह नहीं पा सकती उसी प्रकार मानव मन की ऊँची से ऊँची उड़ान भी परमात्म तत्त्व के अंश मात्र की भी थाह नहीं पा सकती। परंतु मानव और पाशविक चेतना में एक मूलभूत अंतर है सचेतन आरोहण की संभावना का। पशु में हमें इस सचेतन आरोहण की संभावना दिखाई नहीं देती। मनुष्य में इस सचेतन आरोहण की संभावना निहित है और इसका लाभ उठाकर मनुष्य पुनः उस मार्ग का अनुसरण कर के अपने स्रोत तक पहुँच सकता है जिस मार्ग पर अवरोहण करके परम् सत्ता ने इस मानव सत्ता को अपनाया है। और इस आरोहण में सभी सूत्रों, विधि-विधानों, तत्वदर्शनों आदि की तब तक प्रासंगिकता रहती है जब तक कि मानसिक चेतना के द्वारा आरोहण चलता है। गीता भी अपनी शिक्षा के विकासक्रम में गढ़ तत्त्वों को मानसिक भाषा में निरूपित करती है और इस विकास को मन की पराकाष्ठा तक ले जाती है। उसके बाद अपनी शिक्षा का उपसंहार वह 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' के द्वारा कर के सभी मानसिक सूत्रों का सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है और अतिमानस के द्वार तक पहुँच जाती है। परंतु गीता अपनी शिक्षा को वहीं विराम देती है और उससे आगे का वर्णन नहीं करती क्योंकि सभी आधारों का परित्याग करके जब पूरी तरह दिव्य संकल्प अभिव्यक्त होता है तब उसके विधान को किन्हीं भी मानसिक सूत्रों में व्यक्त करना सहज नहीं है और कदाचित् संभव भी नहीं है क्योंकि तब जो विधान सक्रिय होता है वह प्रत्येक के साथ परमात्मा की विशिष्ट क्रिया होती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो केवल अनुभव, अनुभूति आदि के द्वारा ही समझा जा सकता है। हालाँकि, श्रीअरविन्द द्वारा प्रतिपादित चेतना के विभिन्न स्तरों की परंपरा में अतिमानस भी आध्यात्मिक जगतों की श्रेणी में वह पहला ही स्तर है जिसमें कि आत्म-सत्ता उन्मुक्त रूप से स्वयं को अभिव्यक्त कर पाती है। अतिमानस से ऊपर के लोकों में आत्मा की अधिकाधिक भव्यतर और उन्मुक्ततर अभिव्यक्ति संभव होती है जिसमें मानव मन का किसी प्रकार का कोई प्रवेश नहीं है अतः हम उनकी किसी प्रकार की कोई कल्पना तक भी नहीं कर सकते। परंतु चूँकि मानव आत्मा में उन सभी दिव्यतर जगतों की वे सारी भव्यताएँ निहित हैं अतः यह उचित ही है कि आत्मा अपनी उन निहित भव्यताओं को पुनः प्राप्त करे और उन्हें अभिव्यक्त करे। यही इस निम्न अभिव्यक्ति का वास्तविक औचित्य हो सकता है अन्यथा तो इसका अपने आप में कोई औचित्य ही नहीं हो सकता। और इसी दिव्यतर अभिव्यक्ति के लिए श्रीअरविन्द व श्रीमाताजी ने अतिमानसिक अवतरण का उद्घोष किया और उसे केवल किसी दर्शन तक ही सीमित नहीं रखा अपितु उसके लिए आजीवन प्रयास कर सूक्ष्म भौतिक जगत् में उसका अवतरण साधित कराया। उनके अनुसार पार्थिव जगत् की अचेतनता, अज्ञानता आदि सारी समस्याओं का सच्चा अंत केवल अतिमानसिक रूपांतर के द्वारा ही हो सकता है। इस दृष्टिकोण से गीता सभी धर्मों का परित्याग कर के अतिमानस की ओर जाने का मार्ग खोल देती है। जब व्यक्ति अपनी अंतरतम सत्ता में स्वयं परमात्मा है तब वह किन्हीं उच्चतम मानसिक प्रकार के सूत्रों की तो बात ही क्या, अपितु उच्चतम कल्पनीय स्तरों से भी सीमित नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा के सत्स्वरूप को सारा ब्रह्माण्ड और अनेकों सच्चिदानंद भी मिलकर वास्तव में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। निरपेक्ष परमात्म तत्त्व तो वास्तव में इतना निरपेक्ष है कि कोई भी चेतना के उच्चतम स्तर भी उसके लिए बहुत ही गौण विषय हैं। तो ऐसी विलक्षण और अद्भुत उपस्थिति किन्हीं भी सूत्रों में कैसे बंध सकती है। इसी संदर्भ में श्रीमाताजी एक स्थान पर कहती हैं कि व्यक्ति को सदा ही अपने अनुभव की अपेक्षा अधिक उच्च होना चाहिये। जब अपनी सच्ची सत्ता में व्यक्ति स्वयं परमात्मा है तो कैसे किसी भी अनुभव से वह अभिभूत हो सकता है। उच्चतम अनुभूति भी उस परमात्मा के स्वरूप के वैभव को पूरा अनुभूत नहीं कर सकती। इसीलिए सारी योग पद्धतियों आदि का निरूपण करने के बाद गीता सर्वधर्मान्परित्यज्य का परम् मुक्तिदायी वाक्य प्रदान करती है। उसके बाद का क्षेत्र केवल उन्हीं का विषय है जिन्हें उस स्थिति का अनुभव प्राप्त है। और ये सभी सीमाएँ टूटने के बाद भी जीव आत्म-अभिव्यक्ति के लिए, दिव्य संकल्प की अभिव्यक्ति के लिए जगत् में क्रिया करता है। इस भाव में क्रिया का संपूर्ण स्वरूप ही बदल जाता है। कर्म के केवल बाहरी रूप से तो यह पता लगाना भी संभव नहीं होता कि कर्म का उत्प्रेरण कामना आदि निम्न हेतुओं के द्वारा हो रहा है या फिर दिव्य संकल्प द्वारा हो रहा है।
....पहले पाँच श्लोकों में गीता अपना कथन ऐसी भाषा में प्रस्तुत करती है कि वह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संन्यास के मार्गों पर लागू हो सकता है और फिर भी वह उसे ऐसी शैली में उपस्थित करती है कि उसमें से गीता के द्वारा समर्थित पद्धति का अर्थ और भाव निकालने के लिए हमें केवल उन दोनों मार्गों के कुछ सामान्य शब्दों को एक गंभीरतर तथा अधिक अंतर्मुखी अर्थ देना पड़ता है।
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।। ४९।।
४९. सब पदार्थों में आसक्तिरहित बुद्धि, आत्मजयी तथा कामनारहित मनुष्य संन्यास के द्वारा नैष्कर्म्य की परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।
संन्यास, आत्मजय से लब्ध शान्ति, आध्यात्मिक निष्क्रियता और कामना से मुक्ति का यह आदर्श समस्त प्राचीन प्रज्ञा में सामान्य रूप से पाया जाता है। गीता हमें अतुलनीय संपूर्णता और स्पष्टता के साथ इसका मनोवैज्ञानिका आधार प्रदान करती है।
....सक्रिय प्रकृति के गहन बंधन से बाहर निकलने तथा फिर से आध्यात्मिक स्वातंत्र्य लाभ करने का सीधा और सरलतम मार्ग यह है कि जो कुछ भी अज्ञान की क्रियाशक्ति से सम्बन्ध रखता है उस सबको पूर्ण रूप से निकाल फेंक देना और अंतरात्मा को शुद्ध आध्यात्मिक अस्तित्व में रूपांतरित कर देना। इसी को ब्रह्म बनना, 'ब्रह्मभूय' कहा जाता है। इसका अर्थ है निम्नतर मानसिक, प्राणिक और भौतिक अस्तित्व का परित्याग करना और शुद्ध अध्यात्मसत्ता को धारण करना। यह कार्य बुद्धि एवं संकल्प शक्ति के द्वारा सर्वोत्तम रीति से संपन्न किया जा सकता है; यह बुद्धि ही हमारा वर्तमान उच्चतम तत्त्व है। इसे निम्न अस्तित्व की चीजों से और प्रथमतः तथा प्रधानतः अपनी कामनारूपी प्रभावी ग्रंथि से, मन और इन्द्रियाँ जिन विषयों के पीछे दौड़ती हैं उनके प्रति हमारी आसक्ति से दूर हटना होगा। मनुष्य को सभी वस्तुओं में अनासक्त बुद्धिवाला बनना होगा, 'असक्तबुद्धिः सर्वत्र'। तब अपनी नीरवता में प्रतिष्ठित जीव से समस्त कामना दूर हो जाएगी; वह सब लालसाओं से मुक्त, 'विगतस्पृह' हो जाएगा। यह अवस्था अपने संग निम्नतर स्व की अधीनता और उच्चतर स्व की उपलब्धि को ले आती है अथवा उन्हें संभव बना देती है, वह उपलब्धि पूर्ण आत्म-प्रभुत्व पर निर्भर करती है, अपनी परिवर्तनशील प्रकृति पर आमूल विजय और आधिपत्य के द्वारा, 'जितात्मा' बनने के द्वारा, उपलब्ध होती है। और इस सबका अर्थ है वस्तुओं की कामना का पूर्ण आंतरिक त्याग, 'संन्यास'। संन्यास इस पूर्णता का पथ है और जिस मनुष्य ने इस प्रकार आंतरिक रूप से सब कुछ त्याग दिया है उसका वर्णन गीता ने सच्चे संन्यासी के रूप में किया है।.... संन्यास मार्ग क्रियाशील प्रकृति से अपनी निवृत्ति में बहुत ही आगे बढ़ जाता है। वह संन्यास से संन्यास के लिए ही आसक्त रहता है और जीवन और कर्म के बाह्य त्याग और आत्मा तथा प्रकृति की पूर्ण निस्तब्धता पर बल देता है। इसके उत्तर में गीता कहती है कि जब तक हम शरीर में निवास करते हैं तब तक ऐसा पूर्ण रूप से संभव भी नहीं है। जहाँ तक ऐसा करना संभव हो वहाँ तक ऐसा किया जा सकता है, परंतु कर्मों का इस प्रकार कठोरतापूर्वक न्यूनकरण अनिवार्य नहीं हैः यहाँ तक कि वास्तव में या कम-से-कम सामान्यतः यह उचित भी नहीं है। एकमात्र आवश्यक वस्तु है पूर्ण आंतरिक निष्क्रियता और वही गीता के नैष्कर्म्य का संपूर्ण आशय है।...
जब एक बार हमने पूर्णतम आंतरिक निस्तब्धता को शुद्ध निर्व्यक्तिक आत्मा में निवास करने के लिए एक आवश्यक साधन के रूप में मान लिया है तो इसके बाद जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्रियात्मक रूप में निस्तब्धता से यह परिणाम कैसे उत्पन्न होता है।
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।। ५० ।।
५०. हे कुन्तीपुत्र! इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य जिस तरीके से ब्रह्म को प्राप्त करता है, जो मार्ग ज्ञान की परम एकाग्रता का पथ है उस मार्ग को संक्षेप में मुझ से सुन।
यहाँ जिस ज्ञान से अभिप्राय है वह है सांख्यों का योग, - गीता के द्वारा स्वीकृत शुद्ध ज्ञान-योग, 'ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्, जहाँ तक कि यह योग उसके अपने योग के साथ एकीभूत है जिसमें योगियों का कर्ममार्ग भी सम्मिलित है, 'कर्मयोगेन योगिनाम्'। परन्तु यहाँ कर्मों की समस्त चर्चा को वर्तमान के लिए स्थगित रखा गया है। क्योंकि, यहाँ ब्रह्म का सर्वप्रथम अभिप्राय है नीरव, निर्व्यक्तिक एवं अक्षर सत्ता.... सबके साथ और भगवान् तथा उनके विश्वगत संकल्प के साथ एक होने के लिए हमें सबसे पहले निर्व्यक्तिक बनना होगा और अपने अहं तथा उसके दावों से और अपने-आप को, जगत् तथा दूसरों को देखने के अहं के तरीके से मुक्त होना होगा। और यदि हमारी सत्ता में व्यक्तित्व से या अहं से भिन्न कोई और वस्तु न हो, सर्व भूतों के साथ एकीभूत कोई निर्व्यक्तिक आत्मा न हो, तो हम निर्व्यक्तिक और अहं-मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अहं को खोकर यही निर्व्यक्तिक आत्मा बन जाना, अपनी चेतना में यही निर्गुण ब्रह्म बन जाना ही इस योग की पहली गति है। तो भला यह कैसे किया जाए?
बुद्धया विशुद्धया युक्तो घृत्यात्मानं नियम्य च ।
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ।। ५१ ।।
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ।। ५२॥
अहंकारं बलं दर्षं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। ५३।।
५१-५३. शुद्ध की हुई बुद्धि को (अपने भीतर के शुद्ध आत्मतत्त्व के साथ बुद्धियोग के द्वारा) युक्त करके, अपनी सत्ता को सुदृढ़ और अविचल संकल्य से संवत करके, इन्द्रियों के शब्द आदि विषयों का परित्याग करके, मनसे राग एवं द्वेष को दूर हटाकर, निर्जन स्थान में निवास करते हुए, मिताहारी रहते हुए, मन, शरीर एवं वाणी में संयमित, निरंतर ध्यानयोगपरायण, वैराग्य (निष्कामता और अनासक्ति) का पूर्णतया पालन करते हुए, अहंकार, बल, अभिमान, कामना, क्रोध और अधिकृत करने की भावना और सहज-प्रेरणा को छोड़कर, समस्त मैं-पन और मेरे-पन के भाव से मुक्त, शांत मनुष्य ब्रह्म (स्वरूप) बनने के योग्य हो जाता है।
गीता कहती है कि सर्वप्रथम बुद्धियोग के द्वारा अपनी विशुद्ध बुद्धि को अपने अन्दर के शुद्ध अध्यात्म-तत्त्व के साथ योगयुक्त करके, 'बुद्धया विशुद्धया युक्तः,' यह कार्य संपन्न करना होगा। बहिर्मुखी और अधोमुखी दृष्टि से विमुख होकर अंतर्मुखी और ऊर्ध्वमुखी दृष्टि की ओर बुद्धि का यह आध्यात्मिक झुकाव ही ज्ञानयोग का सार है। विशुद्ध बुद्धि को संपूर्ण सत्ता का नियमन करना होगा, 'आत्मानं नियम्य; उसे हमें एक सुदृढ़ और एक धीर संकल्प के द्वारा, 'धृत्या', जो अपनी एकाग्रता में, पूर्ण रूप से, शुद्ध आत्मा की निर्व्यक्तिकता की ओर मुड़ा रहता है, निम्न प्रकृति की बहिर्मुखी कामनाओं के प्रति आसक्ति से परे हटाना होगा। इंद्रियों को अवश्य ही अपने विषयों का त्याग करना होगा, मन को राग-द्वेष अपने अन्दर से निकाल फेंकने होंगे जो कि ये इंद्रिय विषय इसमें भड़काते हैं, क्योंकि निर्व्यक्तिक आत्मा के अन्दर कोई कामनाएँ और जुगुप्साएँ नहीं हैं; ये तो वस्तुओं के स्पर्शों के प्रति हमारे व्यक्तित्व को प्राणिक प्रतिक्रियाएँ हैं, और इन स्पर्शों के प्रति मन और इन्द्रियों का अनुरूप प्रत्युत्तर ही इनका आश्रय और आधार है। मन, वाणी और शरीर पर, यहाँ तक कि प्राणिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं, भूख, सर्दी-गर्मी, शारीरिक सुख-दुःख, पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होगा; हमारी संपूर्ण सत्ता को तटस्थ, इन द्वंद्वों से अप्रभावित, समस्त बाह्य स्पर्शों तथा उनकी आंतरिक प्रतिक्रियाओं एवं प्रत्युत्तरों के प्रति सम बनना होगा। यह सबसे अधिक सीधा और शक्तिशाली तरीका है, योग का सीधा-सटीक और तेज पथ है। कामना और आसक्ति को पूरी तरह से समाप्त होना होगा, 'वैराग्य; साधक से निर्व्यक्तिक निर्जनता में सुदृढ़ रूप से आश्रित होने की और ध्यान द्वारा अंतरतम आत्मा के साथ सतत् ऐक्य लाभ करने की माँग की जाती है। और फिर भी इस कठोर साधना का उद्देश्य विश्व-कर्म में भाग लेने के कष्ट से पराङ्गमुख रहनेवाले मुनि और मनीषी के किसी परम अहमात्मक एकांतवास और शान्ति में आत्म-केंद्रित हो जाना नहीं है; इसका उद्देश्य है समस्त अहं से मुक्त होना।
निर्व्यक्तिकता की यह सर्वप्रथम साधना, जिसका गीता ने उपदेश दिया है, निःसंदेह अपने साथ एक प्रकार की पूर्णतम आंतरिक निष्क्रियता लाती है और अपने अंतरतम भागों में तथा अपने साधनाभ्यास के तत्त्वों में यह संन्यास की प्रणाली के ही समरूप है। और फिर भी एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ क्रियाशील प्रकृति और बाह्य जगत् के दावों के पीछे हटने की इसकी प्रवृत्ति रोक दी जाती है और आंतरिक निष्क्रियता पर एक रोकथाम लगा दी जाती है जिससे कि यह अधिक गहन होकर कर्म-निषेध और भौतिक निवृत्ति" का रूप धारण न कर ले।.... गीता की विचारधारा के इस निर्णायक मोड़ की और अगले दो श्लोकों में संकेत किया गया है, उनमें से पहले का विचारक्रम विशेष रूप से अर्थगर्भित है....
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ।। ५४।।
५४. जब मनुष्य ब्रह्म हो जाता है, जब मनुष्य आत्मा में शांत-प्रसन्न हो न शोक करता है न कामना करता है, जब वह समस्त प्राणियों के प्रति सम हो जाता है तब वह मेरे प्रति परम् प्रेम और पराभक्ति को प्राप्त करता है।
परंतु ज्ञान के संकीर्ण मार्ग में भक्ति, सगुण (personal) ब्रह्म के प्रति भक्ति, केवल एक निम्न एवं प्रारंभिक गति ही हो सकती है; परिणति अथवा पराकाष्ठा तो है निर्गुण ब्रह्म के साथ निर्विशेष एकत्व में व्यक्तित्व का लय जिसमें भक्ति के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकताः क्योंकि वहाँ न कोई उपास्य होता है न कोई उपासक; आत्मा के साथ जीव के निश्चल-नीरख तादात्म्य में और सभी कुछ विलीन हो जाता है। यहाँ गीता में हमें ऐसा कुछ प्रदान किया गया है जो निर्व्यक्तिक ब्रह्म से भी ऊँचा है, - यहाँ है एक परम् आत्मा जो परम ईश्वर है, यहाँ हैं परम् पुरुष और उनकी परमा प्रकृति, यहाँ पुरुषोत्तम जो सव्यक्तिक और निर्व्यक्तिक से परे हैं और अपनी शाश्वत ऊँचाइयों पर इन दोनों में सामंजस्य साधित करते हैं।.... इस दोहरी अनुभूति में ही, सत्ता के अनिर्वचनीय सत्य के दो पक्षों के इस मिलन में ही, जिनमें से किसी एक या दोनों के द्वारा मनुष्य अपनी अनंत सत्ता के पास पहुँच सकता तथा उसमें प्रवेश पा सकता है, मुक्त पुरुष को निवास करना तथा कर्म और अनुभव करना होगा और इसी में उसे सबके साथ तथा अपनी आत्मा के आंतर और बाह्य व्यापारों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने होंगे, या यूँ कहें कि अपनी परमोच्च सत्ता की महत्तम शक्ति के द्वारा उसे अपने लिए उन संबंधों का निर्धारण कराना होगा। और, उस एकीकारक अनुभूति में भी उपासना, प्रीति और भक्ति केवल संभव ही नहीं होतीं, अपितु वे उस उच्चतम अनुभव का एक विस्तृत, अपरिहार्य और सर्वोपरि अंश होती हैं।
प्रश्न : श्लोक संख्या ४९ में भगवान् कहते हैं कि 'सब पदार्थों में आसक्तिरहित बुद्धि, आत्मजयी तथा कामनारहित मनुष्य संन्यास के द्वारा नैष्कर्म्य की परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।' और फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या ५० से ५३ तक भगवान् बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति ब्रह्म बनने के योग्य हो जाता है और ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है तब वह भगवान् के प्रति परम् प्रेम और परमा भक्ति प्राप्त करता है। तो जो अक्षर ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त हो जाता है उसे प्रेम और भक्ति प्रदान करने का क्या औचित्य है?
उत्तर : यह एक बड़ी ही विशिष्ट बात है। जो तथाकथित ज्ञानीजन हैं वे भक्ति या प्रेम आदि भावों को अवमानना की दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दुर्बलता के रूप में देखते हैं और निर्गुण अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति को ही परम् लक्ष्य मानते हैं। परंतु यहाँ गीता भक्ति को तो ब्रह्म की प्राप्ति के बाद की अवस्था बताती है। उसके अनुसार व्यक्ति जब ब्रह्म हो जाता है तब वह भगवान् की पराभक्ति और उनका परम् प्रेम प्राप्त करता है । इसका कारण यह है कि चाहे कितनी भी विशाल बुद्धि हो और उसके माध्यम से कितना भी विशाल और गंभीर अनुभव क्यों न हो, तो भी हृदय सत्य के अधिक निकट जा सकता है। मानसिक अनुभवों में सदा ही एकांगिता रहती है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि सभी तत्वविचारको के अनुभवों के विषय में श्रीअरविन्द का कहना है कि उन सभी के अनुभव निश्चय ही बिल्कुल सही थे परंतु वे सभी थे एकपक्षीय। श्रीअरविन्द कहते हैं कि स्वयं उन्हें भी वे सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं परंतु इनके अतिरिक्त उन्हें असंख्यों और अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। स्वयं श्रीरामकृष्ण परमहंस के उदाहरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार निर्विकल्प समाधि - जिसे कि योग की पद्धतियों में उच्चतम समाधि अवस्था मानते हैं, जिसमें स्थित होने पर व्यक्ति का शरीर इक्कीस दिनों तक ही बने रह सकता है,
-------------------------
* इंद्रियों के द्वारा अपने विषयों का वर्जन, 'विषयांस्त्यक्त्वा', 'त्याग'-रूप ही होना चाहिए; वह अवश्य ही समस्त ऐंद्रिय आसक्ति, 'रस' का परित्याग होना चाहिए, न कि इंद्रियों की स्वभावगत आवश्यक क्रिया का निराकरण। मनुष्य को अपने चारों ओर को वस्तुओं के बीच विचरना होगा और इंद्रिय-क्षेत्र के विषयों पर इंद्रियों के शुद्ध, यथार्थ और प्रगाढ़, सहज और निरपेक्ष व्यापार के साथ क्रिया करनी होगी जिससे कि इन्द्रियाँ दिव्य कर्म में आत्मा के उपयोग में ही आएँ, 'केवलैरिन्द्रियैश्चरन्', कामना की पूर्ति के काम में किंचित्मात्र भी नहीं। वैराग्य अवश्य होना चाहिए, पर जीवन से विरक्ति या जगत्कर्म के प्रति अरुचि के सामान्य अर्थ में नहीं, वरन् राग और साथ ही उसके विपरीत द्वेष के त्याग के अर्थ में। मन और प्राण की समस्त रुचि का और साथ ही उनकी सब प्रकार की अरुचि का भी परित्याग करना होगा। किन्तु गीता हमसे इस चीज की माँग निर्वाण के लिए नहीं, अपितु इसलिए करती है कि एक पूर्ण सामर्थ्यप्रद समता प्रतिष्ठित हो जाए जिसमें आत्मा बस्तुओं के संबंध में सर्वांगीण और व्यापक दिव्य दृष्टि को तथा प्रकृति के बीच सर्वांगीण दिव्य कर्म को एक निर्बाध और अपरिमेय स्वीकृति दे सके।
उसके पश्चात् नष्ट हो जाता है - में छः महीनों तक स्थित रहने के बाद जब वे उस समाधि अवस्था से बाहर आए तो तुरंत ही माँ काली के दर्शनों के लिए मंदिर में चले गए। तोतापुरी जी, जिन्होंने कि उन्हें उस समाधि की दीक्षा दी थी, उनके इस व्यवहार से असमंजस में पड़ गए कि उच्चतम समाधि अवस्था में रहने के बाद भी कैसे कोई व्यक्ति देवी-देवताओं की पूजा-भक्ति आदि कर सकता है क्योंकि उनके अनुसार उसे तो परमोच्च अनुभव प्राप्त हो चुका होता है जिसके बाद भक्ति आदि किन्हीं निम्नतर भावों के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। तब श्रीरामकृष्ण जी की कृपा से उन्हें यह समझ में आया कि माँ जगदम्बा हमारी किन्हीं भी समाधि आदि अवस्थाओं से अनंततः ऊपर और परे हैं।
मानसिक चेतना जब वस्तुओं के सत्य को जानने के लिए असीम निरपेक्ष सत्ता में अपने-आप को प्रक्षिप्त करती है तो परिणामस्वरूप उसे जो आभास प्राप्त होते हैं उन्हें वह ब्रह्म, ईश्वर, सत् आदि की संज्ञाएँ दे देती है। परंतु हमें यह समझना चाहिये कि हमारे ऊँचे से ऊँचे आभास भी बहुत ही सीमित होते हैं और वे परमात्मा को अपनी परिभाषाओं में बाँध नहीं सकते। यह बात तो हम सहज ही समझ सकते हैं कि यदि कोई पाशविक चेतना मानव चेतना का आकलन करने लगे तो वह कभी भी मानव चेतना को समझ कर उसे परिभाषित नहीं कर सकती। परंतु अपने अहं के कारण हमारे लिए अपनी मानसिक चेतना की सीमितता को स्वीकार करना सहज नहीं है। जबकि असीम निरपेक्ष सत्ता तो किन्हीं भी ऊँचे से ऊँचे चेतना के स्तरों से भी कहीं अधिक असीम और निरपेक्ष है। इसी कारण भगवान् श्रीकृष्ण अनेकों बार यह सूचित करते हैं कि वे बहा से, ईश्वर आदि सभी से कहीं अधिक महान् हैं। वे ही ब्रह्म के आधार हैं। अर्थात् भगवान् की चेतना सभी कुछ से परे है। गीता का सारा प्रयास यही है कि सभी मानसिक सूत्रों को सर्वथा त्याग कर उन्हीं भगवान् की शरण ग्रहण की जाए। क्योंकि जब तक व्यक्ति की बुद्धि ब्रह्म में, निर्वाण आदि में ही व्यस्त रहती है तब तक तो वह किसी सच्ची स्थिति में नहीं होता। सभी तत्त्वद्रष्टाओं की परमात्मा के विषय में अपनी-अपनी अवधारणाएँ होती हैं और उन्हें प्रतीत होता है कि वास्तव में उन्हीं का दर्शन सच्चा दर्शन है। और किसी हद तक उनके लिए वह उपयोगी भी हो सकता है, परंतु उनकी अवधारणा से सत्य सीमित नहीं हो सकता। परमात्मा के विषय में सभी के अपने-अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं परंतु वे सारे मिलकर भी परमात्मा के सत्स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकते। अतः सबसे पहले व्यक्ति को गहरे रूप से यह भान होना आवश्यक है कि मानव चेतना में और परमात्म चेतना में बड़ा विशाल अंतर है। परमात्मा के लिए तो चेतना की जिन ऊँची से ऊँची स्थितियों का वर्णन भी हमें पढ़ने और सुनने को मिलता है वह भी एक बहुत ही गौण विषय है क्योंकि आखिर हमारी किन्हीं भी परिभाषाओं में या हमारी किन्हीं भी अनुभूतियों में परमात्मा किसी प्रकार बंध नहीं सकते। गीता की दृष्टि एकमात्र उन परमात्मा के ऊपर है इसीलिए बिल्कुल व्यावहारिक स्तर से आरंभ कर के अपने विकासक्रम में सभी योग-पद्धतियों का निरूपण और समन्वय साधते हुए अंत में गीता उन सभी का अतिक्रमण करके एकमात्र प्रभु की शरण ग्रहण करने की शिक्षा देती है। गीता निष्काम कर्मों के प्रतिपादन से आरंभ करती है, निष्काम कर्म के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। और जब व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है तभी वह परमात्मा के सत्स्वरूप को अधिक अंतरंग रूप से अनुभूत कर सकता है। हालाँकि सच्चा ज्ञान अपने साथ सच्ची भक्ति और सच्चा कर्म भी लिये रहता है, और वास्तव में तो तीनों ही अपने सच्चे रूप में अन्य दो को भी साथ लिये रहते हैं परंतु हमारा हृदय हमारी बुद्धि की बजाय परमात्मा के रहस्य को अधिक अंतरंग रूप से जान सकता है। गीता ने पहले भी यह कहा था कि ज्ञानियों में भी जो भक्ति से युक्त है वह श्रेष्ठ है। अब धीरे-धीरे गीता बड़े ही स्पष्ट रूप से भक्ति को परम् महत्ता प्रदान कर देती है। भगवान् स्पष्ट ही कहते हैं कि 'चूंकि तू मेरा अंतरंग प्रिय है इसलिए मैं तुझे सर्वगुह्यतम रहस्य बताऊँगा।' वे ऐसा नहीं कहते कि 'चूँकि तू परम् ज्ञानी है इसलिए मैं तुझे रहस्य बताऊँगा।' ज्ञान के द्वारा तो व्यक्ति ब्रह्मस्वरूप हो जाता है और ब्रह्मस्वरूप होने पर उसे भगवान् के प्रति प्रेम और परमा भक्ति प्राप्त होते हैं। इस प्रकार गीता भक्ति को परमोच्च स्थान प्रदान करती है।
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ।। ५५।।
५५. अपनी निज सत्ता के यथार्थ स्वरूप और समग्र तत्त्वों में जो मैं हूँ और जितना हूँ, वैसा भक्ति के द्वारा वह मुझे जानने लगता है; इस प्रकार मुझे जानकर वह मुझमें प्रविष्ट हो जाता है।
[गीता कहती है कि भगवान् का पूर्ण ज्ञान] उच्चतम भक्ति से आता है। यह तब प्राप्त होता है जब मन वस्तुओं के संबंध में एक अतिमानसिक और उच्च आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा अपने को अतिक्रम कर जाता है और इसके साथ-ही-साथ जब हृदय भी प्रेम और भक्ति के हमारे अज्ञतर मानसिक रूपों से परे एक ऐसे प्रेम में ऊपर उठ जाता है जो विशालतम ज्ञान से प्रदीप्त, शांत और गंभीर होता है, (और जब हृदय) भगवान् में परम आनंद और अपार भक्ति, अविचल हर्षातिरेक एवं आध्यात्मिक आनंद में ऊपर उठ जाता है। जब जीव ने अपना पृथक् व्यक्तित्त्व खो दिया होता है, जब वह ब्रह्म बन जाता है तभी वह सच्चे पुरुष में निवास कर सकता है और पुरुषोत्तम के प्रति परम उद्भासक भक्ति लाभ कर सकता है और उसकी गंभीर भक्ति तथा उसके हृद्गत ज्ञान की शक्ति के द्वारा उसे पूर्णरूप से जान सकता है, 'भक्त्या मामभिजानन्ति।' यही समग्र ज्ञान है जिसमें हृदय की अगाध दृष्टि मन की चरम अनुभूति को पूर्ण बनाती है, - 'समग्रं मां ज्ञात्वा ।'... इस प्रकार मुक्त पुरुष की अंतरात्मा एक समन्वयकारी ज्ञान के द्वारा पुरुषोत्तम में प्रवेश करती है और एक ही साथ विश्वातीत, व्यक्तिगत तथा विश्वगत भगवान् के पूर्ण आनंद के द्वारा वह उनके अंदर प्रवेश पा लेती है, 'मां विशते तदनन्तरम्।' वह पुरुष अपने आत्म-ज्ञान और आत्मानुभव में, अपनी सत्ता, चेतना और संकल्प में, अपने जगत्-ज्ञान और जगत्प्रेरणा में उनके साथ एक हो जाता है, विश्व में और विश्व के सब प्राणियों के साथ अपने एकत्व में वह उनके साथ एक हो जाता है और साथ ही जगत् और व्यक्ति से परे शाश्वत अनंत की परात्परता में भी, 'शाश्वतं पदमव्ययम्,' वह उनके साथ एक हो जाता है। परम ज्ञान की सारभूत परम भक्ति की चरम परिणति यही है।
और तब यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार अविरत और अविच्छिन्न कर्म, जीवन के कार्य-कलाप के किसी भी भाग को कम किये बिना या छोड़े कमा सब प्रकार का कर्म, न केवल परम आध्यात्मिक अनुभव के साई सर्वथा संगत ही हो सकता है, अपितु वह इस सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने का उतना ही शक्तिशाली साधन भी हो सकता है जितना कि भक्ति या ज्ञान। इस विषय में गीता का जो कथन है उससे अधिक स्पष्ट कथन कोई हो ही नहीं सकता।
यह एक बड़ी ही रोचक बात है कि जिस ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए व्यक्ति सभी कर्मों का त्याग कर पूरी तरह निष्कर्मण्य बन जाता है वही ब्रह्म की प्राप्ति के बाद जब भगवान् के प्रति प्रेम और उनकी पराभक्ति लाभ कर लेता है तब उसके लिए कर्म आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए भक्ति और ज्ञान के समान ही शक्तिशाली साधन बन जाते हैं। इस प्रकार गीता कहीं भी कर्मों के संन्यास का प्रतिपादन नहीं करती। वह तो भक्ति की प्राप्ति के बाद भी कर्मों को उससे समन्वित कर देती है।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः ।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ।। ५६।।
५६. और सर्वदा मुझ में निवास करते हुए सभी कर्मों को करता हुआ भी वह मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी पद प्राप्त करता है।
इस मोक्षप्रद कर्म का स्वरूप उन कर्मों के जैसा है जो हमारे अंदर तथा सृष्टि के अंदर विद्यमान भगवान् के साथ हमारे संकल्प और हमारी प्रकृति के सभी क्रियाशील अंगों के प्रगाढ़ ऐक्य में किये जाते हैं। सबसे पहले यह यज्ञ के रूप में किया जाता है, पर अपने-आप के कर्त्ता होने का भाव अब भी होता है। इसके बाद यह इस भाव के बिना और इस अनुभूति के साथ किया जाता है कि प्रकृति ही एकमात्र कर्ती है। अंत में यह इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि वह प्रकृति भगवान् की परमा शक्ति है, और व्यक्ति को केवल एक माध्यम मात्र एवं एक यंत्र समझकर सभी कर्मों का भगवान् के प्रति संन्यास और समर्पण करते हुए किया जाता है। तब हमारे कर्म सीधे हमारे अंदर स्थित आत्मा और भगवान् से प्रादुर्भूत होते हैं, अविभाज्य विश्व-कर्म का एक अंग होते हैं, हमारे द्वारा नहीं, अपितु एक बृहत् परात्पर शक्ति के द्वारा प्रवर्तित और संपादित होते हैं। तब हम जो कुछ भी करते हैं वह सब सर्वभूतों के हृदय में आसीन प्रभु के लिए, व्यक्ति में अवस्थित परमेश्वर के लिए और हमारे अंदर उनके संकल्प की सिद्धि के लिए, जगत् में विद्यमान भगवान् के लिए. अनभूतों के कल्याण के लिए, जगत्-कर्म और जगत्-उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए, या एक शब्द में, पुरुषोत्तम के लिए किया जाता है और वास्तव में यह साथ अपनी विश्व-शक्ति के द्वारा वे स्वयं ही करते हैं। ये दिव्य कर्म, उनका काही रूप-स्वरूप चाहे जो भी क्यों न हो फिर भी, हमें बाँध नहीं सकते, इसकी बजाय ये तो इस निम्नतर त्रिगुणमयी प्रकृति से परम, दिव्य एवं आध्यात्मिक प्रकृति की पूर्णता की ओर उठने का एक शक्तिशाली साधन हैं। इन मिश्रित और संकीर्ण धर्मों से मुक्त होकर हम उस अमर धर्म में पहुँच जाते हैं जो हम पर तब प्रकट होता है जब हम अपनी समस्त चेतना और कर्म में अपने को पुरुषोत्तम के साथ एक कर लेते हैं। यहाँ हम जो एकत्व लाभ करते हैं वह वहाँ काल से परे अमृतत्व में उठ जाने की शक्ति अपने संग ले आता है। वहाँ हम उनकी नित्य परात्परता में निवास करते हैं।
इस प्रकार ये आठ श्लोक श्रीगुरु के द्वारा पहले ही दिये जा चुके ज्ञान के प्रकाश में ध्यानपूर्वक पढ़ने पर गीता के संपूर्ण योग का संपूर्ण मूलभूत विचार, समग्र केंद्रीय पद्धति और संपूर्ण सार का, भले ही संक्षेप में परंतु फिर भी, एक व्यापक निर्देश करते हैं।
IV. परम्-रहस्य
इस प्रकार शिष्य के सम्मुख उसके कर्म और संग्राम के क्षेत्र में शिक्षा और योग का सार प्रकट कर दिया गया है और अब श्रीगुरु इसे उसके कर्म पर लागू करने की ओर अग्रसर होते हैं, परंतु एक ऐसे ढंग से जिससे यह हमारे समस्त कर्म पर लागू किया जा सकता है। एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण दृष्टांत से संबद्ध और कुरुक्षेत्र के नायक से कहे गए ये शब्द बहुत ही व्यापक अर्थ रखते हैं और जो लोग भी साधारण मानसिकता से ऊपर उठने तथा उच्चतम आध्यात्मिक चेतना में निवास करने और कर्म करने के लिए तैयार हैं उन सभी के लिए ये एक सार्वभौम नियम हैं। अहं और व्यक्तिगत मन के घेरे को तोड़कर उससे बाहर निकल जाना और प्रत्येक चीज को आत्मसत्ता और आत्मा की विशालता में देखना, परमेश्वर को जानना और उनके समग्र सत्य में तथा सभी रूपों में उनकी पूजा करना, प्रकृति और अस्तित्व की परात्पर आत्मा को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, भगवच्चेतना को अधिकृत करना तथा उसके द्वारा अधिकृत होना, प्रेम, आनंद, संकल्प और ज्ञान की सर्व-व्यापकता में उन एकमेवाद्वितीय के साथ एकमय होना, उनके अंदर सभी जीवों के साथ एक होना, एक ऐसे जगत् की दिव्य आधारशिला पर आराधना और यज्ञ के रूप में कर्म करना, जिसमें सभी कुछ भगवान् ही हैं तथा मुक्त आत्मा की दिव्य स्थिति में आराधना और यज्ञ के रूप में कर्म करना - यही गीता के योग का तात्पर्य है। यह है हमारी सत्ता के दृश्यमान सत्य से उसके परम आध्यात्मिक और वास्तविक सत्य में संक्रमण, और, पृथक्कारी चेतना की अनेक सीमाओं को दूर कर और आवेग, चंचलता एवं अज्ञान के प्रति, न्यूनतर प्रकाश और ज्ञान तथा पाप और पुण्य के प्रति, निम्नतर द्वन्द्वात्मक विधान और आदर्श के प्रति मन की आसक्ति का परित्याग करके ही मनुष्य उस सत्य में प्रवेश कर सकता है। इसलिए, श्रीगुरु कहते हैं..
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ।। ५७।।
५७. अपने-आप को पूर्णतया मुझमें अनुरक्त करके, अपने सचेतन मन में अपने समस्त कर्मों को मुझमें समर्पित करके बुद्धियोग का आश्रय ग्रहण करके, सदा अपने हृदय और चेतना में मेरे साथ एक हो।
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि ।। ५८।।
५८. सर्वदा अपने हृदय और चेतना में मेरे साथ एक होकर, मेरी कृपा से तू समस्त कठिन और संकटपूर्ण मागौँ को सुरक्षित रूप में पार कर जाएगा; परंतु यदि तू अहंकारवश नहीं सुनेगा, तो तू नष्ट हो जाएगा।
यह एक बड़ी ही रोचक बात है कि जब व्यक्ति पूर्णतया भगवान् में अनुरक्त हो चुका हो, सचेतन मन में अपने समस्त कर्म भगवान् को अर्पित कर चुका हो और सदा अपने हृदय और चेतना में भगवान् के साथ एक हो चुका हो तब फिर कठिन और संकटपूर्ण मार्ग कौनसे रह जाते हैं। क्योंकि जिन पूर्वस्थितियों की श्रीकृष्ण बात कर रहे हैं - जैसे कि पूर्णतया उनमें अनुरक्त होना, समस्त कर्मों को भगवान् को समर्पित करना आदि – उनमें से किसी एक को भी वास्तव में संसिद्ध करना ही अपने आप में कोई सहज कार्य नहीं है, तब फिर यहाँ वर्णित जब ये सारो ही संसिद्ध हो जाएँ तब तो हमें यही लगेगा कि आखिर करने को शेष रह क्या जाता है। परंतु भगवान् कहते हैं कि ये सब करने के बाद 'मेरी कृपा से तू समस्त कठिन और संकटपूर्ण मागौं को सुरक्षित रूप में पार कर जाएगा। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि हृदय और चेतना में एक हो जाने पर भी जीवन में संकटपूर्ण मार्ग बने रहते हैं परंतु भगवान् की कृपा से व्यक्ति उन्हें पार कर जाता है।
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।। ५९।।
५९. यदि तेरे अहंकार में तू ऐसा सोचता है कि "मैं युद्ध नहीं करूंगा”, तो तेरा निश्चय व्यर्थ है; तेरी प्रकृति तुझे तेरे कर्म में नियुक्त करेगी।
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ।। ६०।।
६०. हे कौन्तेय! मोहवश जिस कर्म को तू नहीं करना चाहता उसे स्वभावजन्य अपने कर्म से बँधा हुआ तू विवश होकर करेगा।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।। ६१।।
६१. हे अर्जुन! ईश्वर समस्त भूतों के हृदय में अवस्थित हैं और अपनी माया के द्वारा यन्त्र पर आरूढ़ के समान समस्त भूतों को घुमाते रहते हैं।
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ।। ६२।।
६२. हे भारत! अपनी सत्ता के समस्त भावों में एकमात्र उन्हीं की शरण ग्रहण कर और उनकी कृपा से तू परा शान्ति और शाश्वत पद को प्राप्त हो जाएगा।
[५७ से ६२ तक के श्लोकों के].... अन्दर इस योग का अंतरतम मर्म निहित है और वे हमें इसके सर्वोच्च अनुभव तक ले जाते हैं और इनको हमें इनके अत्यंत अंतरतम भाव में और उस सर्वोच्च अनुभव की संपूर्ण विशालता में समझना होगा। ये शब्द ईश्वर और मनुष्य के बीच हो सकने वाले अधिक-से-अधिक पूर्ण, घनिष्ठ और जीवंत संबंध को व्यक्त करते हैं; जिन विश्वातीत और विश्वगत भगवान् से मनुष्य उत्पन्न होता है और जिनमें वह वास करता है उनके प्रति उसके अनन्य आराधन, अपनी संपूर्ण सत्ता के ऊर्ध्वमुख समर्पण और निःशेष एवं पूर्ण आत्मदान से जो धार्मिक भाव फूट पड़ता है उसकी घनीभूत शक्ति से ये शब्द ओत-प्रोत हैं। गीता ने भक्ति, ईश्वर-प्रेम और 'परम' की उपासना को श्रेष्ठतम कर्म की अंतरतम भावना और प्रेरणा के रूप में तथा श्रेष्ठतम ज्ञान के मुकुट और सारमर्म के रूप में जो उच्च और स्थायी स्थान दिया है उसके साथ प्रबल भाव पर जोर देना पूर्ण रूप से संगत है। यहाँ जो शब्द प्रयुक्त किये गये हैं और जिस आध्यात्मिक भाव से वे अनुप्राणित हैं वह परमेश्वर के वैयक्तिक सत्य एवं सान्निध्य को संभवनीय गहनतम प्रमुखता और सर्वाधिक महत्ता प्रदान करते प्रतीत होते हैं। यह कोई दार्शनिक की अमूर्त निरपेक्ष सत्ता, सब संबंधों के प्रति असहिष्णु कोई उदासीन निर्व्यक्तिक उपस्थिति या अनिर्वचनीय नीरवता नहीं है जिसके प्रति हमारे सब कर्मों का इस प्रकार का पूर्ण समर्पण किया जा सकता है और हमारे सचेतन अस्तित्व के सभी भागों में उसके साथ एकत्व की इस घनिष्ठता और अंतरंगता को हमारी पूर्णता का अनिवार्य नियम और विधान बनाया जा सकता है, और जिसके कि ये दिव्य सहायता अथवा हस्तक्षेप, संरक्षण और मुक्ति प्रतिज्ञापूर्ण आश्वासन हैं। हमारे कर्मों का प्रभु, हमारी अंतरात्मा का सखा और प्रेमी, हमारे जीवन की अंतरंग आत्मा, हमारी समस्त वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक सत्ता और प्रकृति का अंतर्वासी और ऊर्ध्ववासी अधीश्वर ही एकमात्र वह है जो हमें यह अंतरंग और प्रेरणाप्रद संदेश दे सकता है। तथापि यह वह सामान्य संबंध नहीं है जो धर्मों के द्वारा सात्त्विक या अन्य प्रकार के अहं-मानस में रहनेवाले मनुष्य के तथा इष्टदेव के किसी वैयक्तिक रूप एवं पक्ष के बीच स्थापित किया जाता है, इष्टदेव का यह रूप भी उस मन के द्वारा ही गढ़ा जाता है अथवा यह उसके सीमित आदर्श, अभीप्सा या कामना को पूर्ण करने के लिए उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। वैसा तो सामान्य मानसिक मनुष्य की धार्मिक भक्ति का साधारण आशय एवं वास्तविक स्वरूप है; परंतु यहाँ एक अधिक व्यापक वस्तु विद्यमान है जो मन और उसकी सीमाओं एवं उसके धर्मों को अतिक्रम कर जाती है। मन से अधिक गंभीर कोई सत्ता हो समर्पण करती है और इष्टदेव से अधिक महान् कोई सत्ता ही उस समर्पण को ग्रहण करती है।
यहाँ श्रीअरविन्द एक बड़े ही अद्भुत रहस्य को उजागर करते हैं कि समर्पण करने वाला और समर्पण को ग्रहण करने वाला दोनों बहुत ही गहरी सत्ताएँ होती हैं। समर्पण करने वाले को जो भी कुछ अनुभव होता हो, परंतु कोई गंभीर आंतरिक तत्त्व है जो समर्पण करता है। हालाँकि मानसिक रूप से व्यक्ति का भगवान् के किसी रूप से आकर्षण हो सकता है परंतु श्रीअरविन्द जिस तत्त्व को यहाँ उजागर कर रहे हैं वह समर्पण के किन्हीं मानसिक रूपों से परे है। अतः जो समर्पण करता है वह भी मानसिकता से परे की सत्ता है और जो उसे ग्रहण करता है वह भी इष्टदेवता से कहीं अधिक महान् सत्ता है।
यहाँ जो समर्पण करता है वह है जीव, मनुष्य की मूल अंतरात्मा, उसकी आदि केंद्रीय और आध्यात्मिक सत्ता, व्यष्टि-पुरुष.... गीता की शिक्षा की यही गंभीर व्यापकता है कि जहाँ यह विश्व-भावापन्न निर्व्यक्तिकता के उस सत्य को स्वीकार करती है जिसमें हम अहं के निर्वाण, 'ब्रह्म-निर्वाण' के द्वारा प्रवेश करते हैं, - निश्चय ही इसके बिना मोक्षप्राप्ति संभव नहीं या कम-से-कम कोई चरम मुक्ति संभव नहीं, - वहाँ यह सर्वोच्च अनुभव के अंग के रूप में हमारे व्यक्तित्व के चिरस्थायी आध्यात्मिक सत्य को भी स्वीकार करती है। हमारे अन्दर की यह प्राकृत सत्ता नहीं अपितु वह दिव्य और केंद्रीय सत्ता ही सनातन जीव है। ईश्वर एवं वासुदेव ही, जो कि सब कुछ हैं, हमारे मन, प्राण और शरीर को निम्न प्रकृति के उपभोग के लिए ग्रहण करते हैं; परा प्रकृति, परम् पुरुष की आद्या आध्यात्मिक प्रकृति ही विश्व को संगठित किये हुए है और इसके अन्दर जीव के रूप में प्रकट होती है। अतः यह जीव पुरुषोत्तम की मूल दिव्य अध्यात्म-सत्ता का एक अंश है, जीवंत सनातन की एक जीवंत शक्ति है। वह केवल निम्न प्रकृति का एक अस्थायी रूप नहीं है, अपितु अपनी परा प्रकृति में अवस्थित परमदेव का एक सनातन अंश है, दिव्य अस्तित्व की एक शाश्वत चिन्मय रश्मि है और उतना ही चिरस्थायी है जितनी कि वह परा प्रकृति।
और जो हमारे समर्पण को ग्रहण करता है वह कोई सीमित देवता नहीं, वरन् पुरुषोत्तम है, एकमेव शाश्वत देव, जो कुछ भी है उसकी और समस्त प्रकृति की एकमेव परम् आत्मा, जगत् की आदि परात्पर अध्यात्म-सत्ता है... जो अनिर्वचनीय ब्रह्म है और साथ ही सुहृद्, ईश्वर, प्रकाशदाता और प्रेमी भी है, वही, इस पूर्णतम भक्ति और शरणागति का, इस अत्यंत घनिष्ठ आंतरिक संभूति और समर्पण का पात्र है...
केवल ब्रह्म की ऐकांतिक निर्व्यक्तिकता परमोच्च रहस्य नहीं है। परमोच्च रहस्य तो है यह महान् चमत्कार कि परम् पुरुष और प्रतीयमान बृहत् निर्व्यक्तिक सत्ता - ये दोनों एक ही हैं, सब वस्तुओं का एक अक्षर परात्पर आत्मा और वे परम् पुरुष जो यहाँ अपने-आप को सृष्टि के आधार तक में सर्वत्र कार्यरत एक अनंत और बहुविध व्यक्तित्व के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, - एक आत्मा और पुरुष जो हमारे चरम, अंतरंगतम और गंभीरतम अनुभव में एक निःसीम सत्-स्वरूप पुरुष के रूप में प्रकाशित होते हैं, जो हमें स्वीकार करते हैं और
हमें अपने समीप ले जाते हैं, किसी निराकार अस्तित्व के शून्य में नहीं अपितु अत्यंत प्रत्यक्ष, गंभीर तथा अद्भुत रूप से और अपनी तथा हमारी सचेतन सत्ता के सभी भावों के साथ अपने संपूर्ण निजस्वरूप में ले जाते हैं। यह उच्चतम अनुभूति और देखने का यह व्यापक तरीका हमारी प्रकृति के भागों, हमारे ज्ञान, संकल्प, हृदय के प्रेम और उपासना की एक गंभीर, मर्मस्पर्शी और अनंत सार्थकता प्रकट कर देते हैं, जो कि तब नष्ट या न्यून हो जाती यदि हम केवल निर्व्यक्तिक पर ही एकांगी बल देते, क्योंकि जो प्रवृत्तियाँ और शक्तियाँ हमारी गंभीरतम प्रकृति का एक अंश हैं उनकी गहनतम परिपूर्ति को, उन प्रगाढ़ और तेजोदीप्त स्थितियों को, जो हमारे आत्मानुभव के अंतरतम मूल तंतुओं से बँधी हुई हैं, वह एकांगी बल दबा देता है या लघु-से-लघु कर देता है या फिर संपन्न ही नहीं होने देता। ज्ञान का तप ही एकमात्र वह नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है; उस हृदय के प्रेम और अभीप्सा के लिए भी स्थान है और अनंत स्थान है जो ज्ञान के द्वारा, अधिक गुह्य रूप से सुस्पष्ट, अधिक महान् एवं शांत रूप से भावावेगपूर्ण ज्ञान के द्वारा आलोकित और ऊपर उठा हुआ है। अपनी हृदय-चेतना, मनश्चेतना, समग्र-चेतना के सतत् एकीभूत सान्निध्य के द्वारा ही, सततं मच्चितः, हम सनातन के साथ अपने एकत्व का विशालतम, गंभीरतम एवं पूर्णतम अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ यह उपदेश दिया गया है कि समस्त सत्ता में अंतरंगतम एकत्व ही, जो विश्वभाव के बीच भी, परात्परता के शिखर पर भी दिव्य आवेग के साथ प्रगाढ़ रूप से व्यक्तिगत होता है, मानवात्मा के लिए परम देव की प्राप्ति का पथ है और साथ ही जिस पूर्णता एवं दिव्य चेतना की ओर उसकी प्रकृति उसे आत्मा के रूप में पुकारती है उसे उपलब्ध करने का भी यही मार्ग है। बुद्धि और संकल्प को हमारे संपूर्ण अस्तित्व को उसके सब भागों में ईश्वर की ओर, उस समस्त अस्तित्व के दिव्य आत्मा एवं प्रभु की ओर फेर देना होगा, बुद्धियोगमुपाश्रित्य । हृदय को अन्य समस्त आवेग को उनके साथ एकत्व के आनन्द में परिणत करना होगा, सर्वभूतों में अवस्थित उनके प्रति प्रेम में परिणत करना होगा। इंद्रियों को अध्यात्मभावित होकर सर्वत्र उन्हीं को देखना, सुनना और अनुभव करना होगा। जीवन को पूर्ण रूप से जीव के अन्दर उन्हीं का जीवन बनना होगा। समस्त कर्मों को संकल्प, ज्ञान, कर्मेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों, प्राणिक भागों तथा देह में विद्यमान उनकी अनन्य शक्ति एवं अनन्य प्रेरणा से ही उद्भूत होना होगा। यह मार्ग गहरे रूप से निर्वैयक्तिक है क्योंकि इसमें विश्वभाव तथा पुनः विश्वातीत भाव में प्रतिष्ठित आत्मा के लिए अहं की पृथक्ता मिट जाती है। और फिर भी यह घनिष्ठ रूप से व्यक्तिगत है क्योंकि यह अंतर्निवास तथा हकत्व के लोकोत्तर आवेश एवं शक्ति की ओर उड़ान लेता है। मानसिक तक की कठोर माँग के अनुसार आत्मनिर्वाण का स्वरूप निर्विशेष लय हो सतर्क है, किन्तु वह लय परम रहस्य का, 'रहस्यमुत्तमम्' का अंतिम वचन नहीं है।
हमारी सत्ता में निर्वैयक्तिक भाग भी हैं और सव्यक्तिक भाग भी हैं। और चूंकि प्रत्येक भाग परमात्मा से ही आया हुआ है इसलिए प्रत्येक भाग अपनी तुष्टि और परिपूर्ति चाहता है। यदि व्यक्ति केवल संन्यास, निर्वाण, निवृत्ति आदि पर ही बल दे तो उसके उन भागों को तो स्वयं को तुष्ट और परिपूर्ण करने का अवसर ही नहीं मिल पाता जो परमात्मा के सव्यक्तिक सगुण पक्ष का स्पर्श चाहते हों। इसलिए केवल किसी एक पक्ष को ही तुष्ट करना कभी परम् रहस्य नहीं हो सकता। अधिकांश प्रचलित योग प्रणालियाँ निवृत्ति पर बल देती हैं क्योंकि उनका मानना है कि संन्यास, निवृत्ति आदि के द्वारा व्यक्ति को जब संपर्क प्राप्त हो जाता है तब फिर उसे उसी में स्थित रहना चाहिये और अन्य भागों को उनके अपने हाल पर छोड़ देना चाहिये ताकि धीरे-धीरे उन भागों की वृत्तियाँ या तो शांत हो जाएँगी या नष्ट हो जाएँगी या पोषण के अभाव में क्षीण हो जाएँगी। परंतु जब प्रत्येक भाग को भगवान् का संस्पर्श प्राप्त होता है केवल तभी पूरी सत्ता की परिपूर्णता की पराकाष्ठा होती है। अतः ईश्वर की सत्ता व्यक्तित्वशून्य नहीं हो सकती। यदि ईश्वर व्यक्तित्वशून्य होते तो कहीं भी कोई व्यक्तित्व आ ही कैसे सकता था। व्यक्तित्व और निर्व्यक्तित्व के विषय में योगी श्रीकृष्णप्रेम द्वारा लिखे पत्र बड़े ही प्रकाशक हैं। वे कहते हैं, "व्यक्तित्व तथा निर्व्यक्तित्व जैसे झगड़ों से अपने को व्यथित मत करो। व्यक्तित्व का अपने ठीक विपरीत निर्व्यक्तित्व से अलग अपने-आप में कोई अर्थ नहीं है और ऐसा ही निर्व्यक्तित्व के साथ है। वे तो मानसिक शब्द हैं और विचार में सदा ही एक दूसरे से संयुक्त किये जाने चाहिये। चेतना में किसी एक पर अतिशय बल देने का अर्थ है दूसरे की घातक प्रतिच्छाया द्वारा परेशान किये जाना। दोनों ही क्रियाओं के प्रति ग्रहणशील रहो, और कृष्ण, जिनसे दोनों ही उत्पन्न होते हैं, आत्मा को फलप्रद बनाएँगे।" (योगी श्रीकृष्णप्रेम, पृष्ठ २१६)
एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं कि, "मैं स्वयं पूर्णतः सुनिश्चित हूँ कि श्रीकृष्ण को पूर्ण मूर्तता या ठोस रूप में अनुभव किया जा सकता है। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मैंने एक बार पहले भी यह बताया था, वे तो सभी मूर्तताओं के परम् मूर्त हैं न कि महज़ कोई कोहरेनुमा धुँधले अमूर्त या काल्पनिक रूप हैं। वे किसी निराकार ब्रह्म में से कोई अर्थ-काल्पनिक प्रक्षेपण नहीं हैं, वरन् वह सद्वस्तु हैं जो अन्य सभी कुछ को अवलंब प्रदान करती है। मैं निर्विशेष ब्रह्म के अनुभव की सत्यता को अस्वीकार नहीं कर रहा अपितु यह कह रहा हूँ कि उसे देखना तो सूर्यप्रकाश को देखने के समान है जबकि कृष्ण को देखना स्वयं सूर्य को देखना है।
मैं तुमसे सर्वथा सहमत हूँ कि श्रीकृष्ण का प्रेम किसी भी मात्र नियक्तिक आनंद से कहीं अधिक परिपूरक या तुष्टिप्रद है और जो कोई ऐसे प्रेम की कामना करने के स्तर तक भी पहुँच गया, वह उससे कम में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। परंतु वहीं दूसरी ओर, मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि हमें उन पर यह माँग भी नहीं लादनी चाहिये कि हमारे प्रेम को ग्रहण करने के लिए उन्हें अपने-आप को दिखाना चाहिये। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि वे ऐसा कर सकते हैं और करते ही हैं, और वह भी उतने ठोस रूप में जितना कि कोई उनसे कामना कर सकता था, परंतु मुझे लगता है कि व्यक्ति को यह पूर्ण रूप से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिये और - यदि यही उनकी इच्छा हो तो - बिना किसी प्रतिफल के अथवा यहाँ तक किसी दर्शन के बिना भी उनसे प्रेम करने में संतुष्ट रहे। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हमारा प्रेम स्वार्थ में रंगा रहता है। गोपीप्रेम कृष्ण का रस लेने या उनका भोग करने की कामना नहीं है बल्कि वह तो उनकी सेवा करने और उनके द्वारा उपभोग किये जाने की कामना है। व्यक्ति को कोई भी माँग और कोई भी सौदेबाजी या मोलभाव नहीं करना चाहिये। परंतु इसके साथ ही इसका यह अर्थ नहीं है, जैसा कि कुछ आध्यात्मिकरण करने वाले लोग शिक्षा देते हैं, कि कृष्ण का प्रेम तो इस प्रकार सहज रीति से निःस्वार्थता को अवस्था को प्रतिष्ठित करने का महज़ एक साधन है और यह कि जब वह प्राप्त हो जाए तो फिर सगुण-साकार व्यक्तिगत कृष्ण की आगे और कोई आवश्यकता नहीं है। बात तो इससे ठीक उल्टी है। निःस्वार्थता तो उन्हें प्राप्त करने का साधन है और उनके अपने समय पर वे अपने भक्त के प्रेम को उतने ही व्यक्तिगत और यथार्थ रूप में स्वीकार करते हैं जितना कि कोई उनसे कामना कर सकता था, और हम कल्पना भी कर सकें उससे भी कहीं अधिक वास्तविक रूप से वे स्वीकार करते हैं। वे तो, जैसा कि तुम कहते हो, 'दृष्टिपटल पर पड़े सूर्यप्रकाश' से भी अधिक वास्तविक और अधिक जीवंत हैं। हम आध्यात्मिक यथार्थताओं को अस्पष्ट और भारहीन मानने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि यह बोध करने में सर्वथा असफल रहते हैं कि हमारे इंद्रियानुभवों में जो भी 'यथार्थता' और 'जीवंतता' हम पाते हैं वह तो और कुछ नहीं केवल उनकी जीवंतता की एक क्षीण-सी छाया ही तो है। श्रीकृष्ण के आलिंगन पुरुष और प्रकृति के विषय में कोई बेकार रूपक नहीं हैं। और भगवान् के लिये दिलीप, यह याद रखो कि कृष्ण के चरण तुम्हारे अपने पैरों से अधिक यथार्थ अथवा वास्तविक हैं।" (योगी श्रीकृष्णप्रेम, लेखकः दिलीप कुमार रॉय, श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट, पृष्ठ १६९-७०)
स्वयं गीता भी ब्रह्म निर्वाण आदि स्थितियों से गति करते हुए अंत में भगवान् के सव्यक्तिक स्वरूप पर ही आती है। अपनी सत्ता को प्रतिष्ठित करते हुए भगवान् स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सब कुछ का परित्याग कर के मेरी शरण में आ जा। स्वयं श्रीअरविन्द भी अपनी साधना में इसी पक्ष पर बल देते हैं। श्रीरामकृष्णजी की जीवनी में भी हमें देखने को मिलता है कि छः महीने निर्विकल्प समाधि में स्थित रहने के बाद भी समाधि अवस्था से बाहर आते ही उन्होंने माँ काली के मंदिर में जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रचलित योग पद्धतियों के अनुसार तो ब्रह्म के अनुभव के बाद व्यक्ति को उच्चतम स्थिति प्राप्त हो जाती है और उसके बाद किसी सव्यक्तिक स्वरूप की आवश्यकता ही नहीं रहती। परंतु श्रीरामकृष्णजी ने स्वयं यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म आदि अनुभूतियाँ तो माँ जगदंबा की ही कृपा से प्राप्त होती हैं और जगदंबा स्वयं इन सभी अनुभूतियों आदि से सर्वथा ऊपर और परे बनी रहती हैं। सारा भारतीय तंत्र भी इसी सव्यक्तिक स्वरूप पर आग्रह रखता है। वास्तव में परमात्मा सव्यक्तिक और निर्व्यक्तिक की हमारी सभी अवधारणाओं से सर्वथा परे हैं और दोनों ही पक्ष मिल कर ही हमारे लिए उनके स्वरूप को परिपूर्ण बनाने की तरफ गति कर सकते हैं।
अपने भगवन्नियोजित कर्म में प्रवृत्त होने से अर्जुन का इन्कार उसके अंदर के अहंकार के कारण हुआ था। परंतु इसके पीछे था सात्त्विक, राजसिक और तामसिक अहं के विचारों और प्रवृत्तियों का मिश्रण, उनकी अस्तव्यस्तता और विषम भ्रांति, प्राणिक प्रकृति का पाप और उससे होने वाले व्यक्तिगत परिणामों का भय, हृदय का व्यक्तिगत शोक और संताप से पीछे हटना, आच्छादित बुद्धि का धर्म और पुण्य की आत्मप्रवंचनामय सत्याभासी पुकारों के द्वारा अहंकारमय आवेगों के समर्थन का आवरण, हमारी प्रकृति का भगवान् की कार्यशैलियों से अज्ञानपूर्वक इसलिए सिकुड़ना क्योंकि वे मनुष्य की शैलियों से भिन्न प्रतीत होती हैं और उसके स्नायविक तथा भावावेगमय अंगों पर एवं उसकी बुद्धि पर भीषण और अप्रिय चीजों को लादती हैं। अब जब कि एक उच्चतर सत्य, कर्म का एक महत्तर तरीका और भाव उसके समक्ष प्रकट किया जा चुका है, फिर भी यदि वह अपने अहंभाव पर दृढ़ रहकर कर्म न करने के व्यर्थ और असंभव निश्चय पर डटे रहता है, तो इसके आध्यात्मिक परिणाम पहले की अपेक्षा अब और भी अनंतगुना अनिष्टकारी होंगे। क्योंकि यह एक मिथ्या निश्चय है, एक व्यर्थ पराङ्गमुखता है, क्योंकि यह केवल एक अस्थायी दुर्बलता से, उसके अंतरतम स्वभाव की शक्ति के विधान से एक प्रबल पर अस्थायी रूप में विचलित होने से उत्पन्न हुआ है जो कि उसकी प्रकृति का सच्चा संकल्प और पथ नहीं है। यदि अब वह अपने अस्त्र-शस्त्र फेंक दे तो भी जब वह देखेगा कि युद्ध और संहार उसके बिना भी चल ही रहे हैं, उसकी पराङ्गमुखता के फलस्वरूप उन सब चीजों की, जिनके लिए उसने जीवन बिताया है, पराजय हो रही है, जिस ध्येय की सेवा के लिए उसका जन्म हुआ था वह अपने नायक की अनुपस्थिति या अकर्मण्यता के कारण दुर्बल और पथभ्रांत हो रहा है, स्वार्थपरायण अधर्म और अन्याय के समर्थकों की विद्वेषपूर्ण और विवेकहीन शक्ति के द्वारा पराजित और उत्पीड़ित हो रहा है तो उसे उसकी अपनी प्रकृति ही पुनः शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देगी। और इस वापसी से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। यह केवल अहंमय मन की धारणाओं और भावनाओं का संभ्रम ही था जिसने उसे इन्कार करने के लिए प्रेरित किया था; अहंमय मन की विशिष्ट धारणाओं और भावनाओं की पुनः प्रतिष्ठा के द्वारा कार्य करती हुई उसकी प्रकृति हो उसे अपने इन्कार को रद्द करने के लिए विवश करेगी। परन्तु चाहे किसी भी दिशा में क्यों न हो, इस प्रकार अभी भी अहं के वश में रहने का अर्थ होगा और भी बुरा, और भी घातक अध्यात्म-निषेध, 'विनष्टि; क्योंकि यह, निम्न प्रकृति के अज्ञान में [इस प्रकार युद्ध करने या नहीं करने में] उसने अपनी सत्ता के जिस सत्य का अनुसरण किया है उसकी अपेक्षा एक महत्तर सत्य से [जो उसके सामने दिव्य गुरु द्वारा प्रकट किया जा चुका है। एक निश्चित पतन होगा। उसे एक उच्चतर चेतना में, एक नये आत्म-साक्षात्कार में प्रवेश प्राप्त हो चुका है, अहंकारमय कर्म के स्थान पर दिव्य कर्म करने की संभावना उसे दिखायी जा चुकी है; एक निरे बौद्धिक, भावनाप्रधान, ऐन्द्रिय और प्राणिक जीवन के स्थान पर एक दिव्य आध्यात्मिक जीवन के द्वार उसके सामने खोल दिए गये हैं। उसे आह्वान प्राप्त हो चुका है कि वह अब और एक महान् अंधा यंत्र न रहे अपितु एक सचेतन आत्मा तथा भगवान् की एक ज्ञानदीप्त शक्ति एवं उनका पात्र बने।
अचेतनतावश यदि कोई त्रुटि करता है तो उसके अपने परिणाम हैं। परंतु वहीं यदि व्यक्ति सचेतन होकर त्रुटि करता है तब उसके परिणाम तो अनंतगुना अधिक अनिष्टकारी होते हैं। अतः जिन लोगों को अपने जीवन में किसी गहरी चीज की कोई अनुभूति नहीं हुई है, जिनमें किसी महत् कार्य के प्रति या किसी उच्चतर उद्देश्य के प्रति कोई अभीप्सा नहीं है उनके लिए तो सहज ही है कि वे सुचारू रूप से अपना प्राणिक-भौतिक जीवन जीते रहें जिसमें कि कामना ही सर्वोपरि चालक शक्ति होती है। ऐसे लोग यदि अपनी सुखभोगवादी प्रवृत्तियों की तुष्टि करते हैं तो वह तो उनकी प्रकृति के लिए सहज ही है। परंतु यदि व्यक्ति को किसी गहरी चीज का, किसी गहरे भाव का, किसी गंभीर अभीप्सा का संस्पर्श या स्पंदन प्राप्त हो चुका है और फिर भी वह उसकी उपेक्षा करके उन्हीं निम्नतर प्रवृत्तियों की ही तुष्टि में लगा रहता है तब उसके लिए इसके बड़े ही गंभीर परिणाम उत्पन्न होते हैं। अतः सचेतनता आने के साथ व्यक्ति का दायित्व बढ़ जाता है। जीवन में भी हम देखते हैं कि एक अबोध बालक की त्रुटि को हम अनदेखा कर सकते हैं वहीं किसी वयस्क की त्रुटि के लिए हम उसके सुधार या दण्ड की दिशा में आवश्यक कदम उठाते हैं। चेतना की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि जिसकी चेतना अत्यधिक विकसित होती है उसके ऊपर सहज ही दिशानिर्देश का, मार्गदर्शन का कार्यभार आ जाता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में ऋषि शीर्षस्थ व्यक्ति होता था। चूंकि वह स्वयं अपने आत्मा के विधान द्वारा शासित होता था जिससे विचलित होने के अपने भयंकर अनिष्टकारी परिणाम होते थे अतः उस पर किन्हीं बाहरी नियमों को लादने का कोई विधान ही नहीं था क्योंकि यह सुविज्ञात था कि किसी द्विज के ऊपर या किसी विप्र आदि के ऊपर उसकी आत्मा का विधान किन्हीं भी बाहरी विधानों से कहीं अधिक बाध्यकारी होता है। इसीलिए श्रीअरविन्द कहते हैं कि अब जबकि अर्जुन की सभी जिज्ञासाओं को शान्त कर दिया गया है, उसे चेतना में विकसित किया जा चुका है तब यदि वह कर्म न करने के अपने अहंमय निश्चय पर डटा रहता है तो उसके भयंकर रूप से अनिष्टकारी आध्यात्मिक परिणाम होंगे। यही नहीं, अपनी प्रकृति द्वारा बाध्य होकर जब उसे अवश रूप से युद्ध करना पड़ेगा तो उसमें भी कोई आध्यात्मिक हित नहीं होगा क्योंकि बाहरी परिस्थितियों से बाध्य होकर कर्म करने में किसी प्रकार का कोई श्रेष्ठ हित नहीं हो सकता। जहाँ भगवान् के प्रेम से अभीभूत होकर कर्म करने से व्यक्ति को परम् आनन्द प्राप्त होता है और सारी सत्ता उससे पुलकित हो उठती है और शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण होता है, वहीं यदि बाध्य होकर व्यक्ति को कर्म करना पड़े तो यह उसकी सत्ता की शक्तियों को क्षीण कर देता है और उसके अपने अंदर ही एक प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न कर देता है। सचेतन रूप से कर्म करने में और बाध्य होकर कर्म करने में यही अंतर है अन्यथा कर्म तो बोझे का पशु भी बहुत करता है परंतु उसमें किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक श्रेय नहीं होता। यदि कर्म का अभिप्राय बाहरी क्रियाओं से ही मानें तब तो हमें पशु को भी कर्मयोगी की संज्ञा देनी चाहिये, परंतु उसके कर्म को हम योग नहीं कहते क्योंकि योग तो एक सहर्ष सचेतन आत्मदान की क्रिया है जो किसी भी बाहरी कारण से बाध्य होकर कर्म करने tilde 7 नहीं हो सकती। अतः कर्म के बाहरी स्वरूप से नहीं अपितु उसकी चालक शक्ति के ऊपर उसका भीतरी परिणाम निर्भर करता है। अर्जुन ने भी अपनी निम्न प्रकृति के दबाव के कारण युद्ध से मना कर दिया था और उसी निम्न प्रकृति से बाध्य होकर यदि वह कर्म में प्रवृत्त होता है तो इसमें किसी प्रकार से कोई श्रेयस्कर कार्य नहीं होगा।
प्राणीमात्र के हृदय में अवस्थित ईश्वर ही हमें हमारी अज्ञानावस्था के समस्त आंतरिक और बाह्य कर्म में निम्न प्रकृति की इस माया के पहिये पर यंत्रारूढ़ की भाँति घुमाते आ रहे हैं। और चाहे अज्ञान में तमसाच्छन्न अवस्था में हो या ज्ञान में उद्दीप्त, हमारे अन्दर तथा जगत् के अन्दर अवस्थित उन ईश्वर के लिए ही हमारा अस्तित्व है। इस ज्ञान और इस सत्य में सचेतन तथा सर्वांगीण रूप से निवास करने का अर्थ है अहं से मुक्त होना तथा माया के घेरे को तोड़कर उससे बाहर निकलना। अन्य सभी उच्चतम धर्म इस धर्म के लिए एक तैयारी मात्र हैं, और समस्त योग केवल एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी सत्ता के अधीश्वर और परम् पुरुष एवं आत्मा के साथ पहले किसी-न-किसी प्रकार का मिलन और अंत में, यदि पूर्ण ज्योति प्राप्त हो तो, सर्वांगीण मिलन लाभ कर सकते हैं। महानतम योग है अपनी प्रकृति की सब दुविधाओं और कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण प्रकृति के उन अंतर्वासी ईश्वर की शरण लेना, अपनी संपूर्ण सत्ता सहित, प्राण, शरीर, इंद्रिय, मन, हृदय और बुद्धि सहित, उसी के प्रति अर्पित अपने संपूर्ण ज्ञान, संकल्प और कर्म के सहित, 'सर्वभावेन', अपने सचेतन स्वत्व और यंत्रात्मक प्रकृति के सभी भावों के सहित उन्हीं अंतर्वासी ईश्वर की ओर मुड़ना। और जब हम सदा-सर्वदा तथा पूर्ण रूप से ऐसा कर सकेंगे, तब दिव्य ज्योति, प्रेम और शक्ति हमें अपने अधिकार में कर लेगी, हमारी सत्ता और हमारे उपकरणों को दोनों को परिपूर्ण कर देगी और हमारे अंतःकरण तथा जीवन को घेरने वाले समस्त संदेहों, कठिनाइयों, दुविधाओं और विपदाओं में से हमें सुरक्षित ले चलेगी, हमें परा शांति और हमारे अमर एवं शाश्वत पद की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी, परा शान्तिम्, स्थानं शाश्वतम्।
प्रश्न : यहाँ श्लोक संख्या इकसठ में भगवान् कहते हैं कि 'ईश्वर समस्त भूतों के हृदय में अवस्थित हैं' परंतु वे ही भगवान् माया में डालकर समस्त भूतों को यन्त्र पर आरूढ़ के समान घुमाते रहते हैं। तो व्यक्ति को करने का कार्य है 'तमेव शरणं गच्छ' अर्थात् 'उसी की शरण ग्रहण कर'। अब इसमें दो बातें हैं- यदि भगवान् स्वयं ही भीतर विराजमान हैं तो फिर सभी भूतों को भ्रम में क्यों डाल रखा है और दूसरे सर्वभावेन उनकी शरण ग्रहण करने से क्या अर्थ है?
उत्तर : जब व्यक्ति उस उपस्थिति के विषय में सज्ञान नहीं होता तभी उसे यंत्रवत् चलाया जाता है। परंतु जब वह उस उपस्थिति के विषय में सचेतन हो जाता है और उसके प्रति भाव रखने लगता है तब वह सचेतन रूप से उन ईश्वर के पास जा सकता है। यह अंतर वैसा ही है जैसे कि कोई या तो प्रेम के कारण किसी की सेवा करे या फिर केवल किसी लाभ की आशा से बाध्य होकर सेवा करे। दोनों की भावना में बड़ा भारी अंतर होगा। और जब सर्वभावेन व्यक्ति ईश्वर की शरण ग्रहण कर लेता है तब वह सभी भयों, प्रताड़नाओं आदि से मुक्त होकर पराशान्ति और शाश्वत पद प्राप्त कर लेता है।
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।। ६३।।
६३. यह मैंने तुझे गुद्ध से भी गुच्चतर ज्ञान कहा है; इस पर पूर्णतया विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर।
सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ।। ६४ ।।
६४. और भी, मेरे परम वचन को, सबसे गुह्यतम सत्य को सुन; तू मेरे लिए अंतरंग प्रिय है, इसलिए इसे मैं तेरे उच्चतम कल्याण के लिए इसे कहता हूँ।
क्योंकि, समस्त धर्मों का और अपने योग के गहनतम सार का प्रतिपादन करने के बाद, यह बताने के बाद कि आध्यात्मिक ज्ञान के रूपांतरकारी प्रकाश के द्वारा मानव-मन के समक्ष प्रकाशित सभी प्राथमिक रहस्यों के परे, 'गुह्यात्', यह एक और भी गंभीर एवं गुह्यतर सत्य है, 'गुह्यतरम्', गीता एकदम ही यह कहती है कि अभी भी एक परम वचन, 'परमं वचः', है जो उसे कहना है, और अभी भी एक सर्वाधिक गुह्य सत्य है, 'सर्वगुह्यतमम्'। यह रहस्यों का रहस्य श्रीगुरु अर्जुन को उसके सर्वोच्च कल्याण के रूप में बतलाएँगे क्योंकि वह उनकी चुनी हुई और प्रिय आत्मा है, उनका 'इष्ट' है। क्योंकि स्पष्ट ही, जैसा कि उपनिषद् पहले ही घोषित कर चुका है, अपने वास्तविक स्वरूप को, 'तनुं स्वाम्', प्रकाशित करने के लिए परमात्मा के द्वारा चुना हुआ कोई विरला जीव ही इस रहस्य में प्रवेश पा सकता है, क्योंकि केवल वही हृदय, मन और प्राण में परमेश्वर के इतना पर्याप्त निकट होता है कि वह अपनी सारी सत्ता में उन्हें सच्चे रूप में प्रत्युत्तर दे सकता है अथवा उनके अनुकूल हो सकता है तथा उसे अपना जीवंत अभ्यास बना सकता है। गीता का अंतिम उपसंहार-रूप परम वचन, जो उच्चतम रहस्य को प्रकट करता है, दो संक्षिप्त, सुस्पष्ट और सरल श्लोकों में कहा गया है और इनकी और आगे व्याख्या या विस्तार किये बिना इन्हें मन के भीतर गहरे जाकर आत्मा की अनुभूति में अपना पूर्ण अर्थ प्रकाशित करने के लिए छोड़ दिया गया है। क्योंकि एकमात्र यह निरन्तर विस्तृत होनेवाली आन्तरिक अनुभूति ही है जो ऊपर से इतने साधारण एवं सीधे-सादे लगने पर भी जिस अनंत अर्थ-गौरव से नित्यगर्भित ये शब्द हैं उसे स्पष्ट कर सकती है। और जब ये शब्द उच्चारित होते हैं तो हमें अनुभव होता है कि यही चीज है जिसके लिए शिष्य की आत्मा को इस पूरे समय में तैयार किया जा रहा था और शेष सब तो केवल एक ज्ञानोद्दीपक और सामर्थ्यप्रद साधना एवं शिक्षा थी। यह है रहस्यों का रहस्य, ईश्वर का सर्वोच्च स्पष्टतम संदेश।
जब गीता 'सर्वगुह्यतमं' वाक्य प्रदान करने की बात करती है तब इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी गीता तो इस रहस्य तक पहुँचने की एक तैयारी मात्र थी। वह तो इस स्थिति तक लाने के लिए अर्जुन को पर्याप्त रूप से विकसित कर रही थी ताकि उसे यह परम् वचन दिया जा सके। अब अर्जुन को जो उपदेश दिया जाना है वह सभी मानसिक नियमों को छिन्न-भिन्न करके उनसे सर्वथा परे चला जाता है। बाकी सारी शिक्षा तो केवल मानसिक धरातल पर चल रही थी, जबकि जो ज्ञान अब आने वाला है वह मन से अगम है जिसे मन से नहीं समझा जा सकता और न ही उसकी कोई कल्पना ही की जा सकती है। और मन से मुक्त होने पर व्यक्ति मनुष्यता से ऊपर उठ जाता है।
प्रश्न : श्लोक इकसठ में भगवान् कहते हैं कि ईश्वर सब भूतों को यंत्रारूढ़ के समान घुमाते हैं और दो श्लोकों बाद ही भगवान् अर्जुन को कहते हैं कि तेरी इच्छा हो वैसा कर, तो जो यंत्रवत् चलता है वह अपनी इच्छा से निर्णय कैसे कर सकता है?
उत्तर : वास्तव में तो केवल ईश्वर की ही इच्छा कार्यान्वित होती है परंतु मूढ़ जनों को यह भ्रम हो जाता है कि वे स्वयं कुछ कर रहे हैं। इसीलिए भगवान् अर्जुन से कहते हैं कि जो होना है वह तो तय है और उसे तो केवल निमित्त बनना है, परंतु इतने पर भी यदि अपनी निम्न प्रकृति के अहंवश वह अपने हठ पर बना रहता है तो उसी प्रकृति द्वारा वह युद्ध करने को बाध्य होगा। परंतु इस बाध्यतावश युद्ध करने में कोई श्रेय नहीं होगा। अब इसमें देखने की बात यह है कि भगवान् ने अर्जुन के निर्णय की कोई प्रतीक्षा किये बिना ही उसे अपना सर्वगुह्यतम वचन प्रदान कर दिया चूंकि वह उनका अंतरंग था। इसमें यदि मान लें कि भगवान् अर्जुन के उत्तर की प्रतीक्षा करते, तो भी निःसंदेह वह भी भगवद्प्रेरणा से प्रेरित होकर युद्ध में प्रवृत्त होने का चयन करता परंतु तब कदाचित् परम् वचन को सुनाने का अवसर ही उत्पन्न न होता जिसके लिए कि सारी गीता एक तैयारी मात्र ही थी। इसीलिए भगवान् बीच में कोई भी अवसर प्रदान किये बिना सीधे ही अपनी शिक्षा का सर्वगुह्यतम सत्य उद्घाटित कर देते हैं।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।। ६५।।
६५. मेरे मनवाला, मेरा प्रेमी और उपासक, मेरे प्रति यज्ञ करनेवाला बन, मुझे नमस्कार करः तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा, यह तुझे मेरा वचन और मेरी प्रतिज्ञा है क्योंकि तू मुझे प्रिय है।
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। ६६।।
६६. समस्त धर्मों का परित्याग कर और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर। मैं तुझे समस्त पाप और बुराई से मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर।
जिसे भगवान् अपना सर्वगुह्यतम वचन कहते हैं वह सतही रूप से सुनने में ऐसा सहज लगता है कि बिना गहरे अनुभव के इसे और इससे पूर्व की गीता की शिक्षा की गहराई में भेद कर पाना संभव ही नहीं है। केवल श्रीअरविन्द की टीका ही इस परम् रहस्य को उजागर करती है अन्यथा भगवान् के द्वारा स्वयं यह स्पष्ट रूप से कहे जाने पर भी कि उनका सर्वगुह्यतम वचन क्या है, अधिकांश टीकाकार तो गीता के प्रारंभिक अध्यायों को ही गीता का सारमर्म घोषित कर देते हैं। और यह त्रुटि करना सहज ही है क्योंकि इस वचन के निहितार्थ या इसके गूढ़ार्थ तो साधना आदि सभी पद्धतियों की परिणति हैं इसीलिए ये हमारे ऊँचे से ऊँचे अनुभवों से भी छूट निकलते हैं। और जब श्रीअरविन्द कहते हैं कि संपूर्ण गीता केवल इन दो श्लोकों को प्रदान करने के लिए तैयारी मात्र थी, तो सामान्यतः इस कथन में अतिशयोक्ति प्रतीत होती है कि जहाँ पूर्व में भगवान् गंभीर तत्त्वज्ञान, विभिन्न योग पद्धतियों आदि का निरूपण कर चुके हैं उनकी तुलना में तो यह उक्ति बिल्कुल सीधी-सरल प्रतीत होती है। और यदि भगवान् को अंततः यही कहना था कि सभी कुछ का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, तो यह बात तो वे आरंभ में ही कह सकते थे। फिर इतनी योग पद्धतियों आदि का निरूपण करने की आवश्यकता ही क्या थी। जिसे भगवान् परम रहस्य कह रहे हैं उसमें तो कोई रहस्य की बात ही प्रतीत नहीं होती, अपितु यह तो एक बड़ी ही सीधी-सीधी बात प्रतीत होती है कि सब कुछ भगवान् को समर्पित कर दो। यह उक्ति तो बड़ी ही सामान्य प्रकार की उक्ति है जो प्रायः ही हमें किसी सामान्य व्यक्ति से भी सुनने को मिल सकती है। तब फिर भगवान् को इसे इतने सनसनीखेज तरीके से बताने की क्या आवश्यकता थो। और यदि यही कहना था कि सभी कुछ का परित्याग कर दो, तब फिर यह तो अन्य योग-साधनाओं की तुलना में बड़ा ही सरल मार्ग है जिसमें कुछ भी श्रम की आवश्यकता नहीं है अन्यथा तो योग पद्धतियों में बहुत ही अधिक श्रम होता है। यही नहीं, इससे आगे भगवान् कहते हैं कि जो तप से या भक्ति से विहीन है, जिसे सुनने की इच्छा नहीं है अथवा जो उनकी निन्दा करता है और उन्हें गौण समझता है उसे यह ज्ञान नहीं देना चाहिये। और इन मानकों के आधार पर तो इस ज्ञान का कदाचित् ही कोई सच्चा अधिकारी मिलेगा। और आखिर इसमें ऐसा कौनसा रहस्यमय तत्त्व है जिसे कि अनधिकारी को नहीं देना चाहिये? इसका कारण तो स्पष्ट है कि अनधिकारी को यह ज्ञान देने पर वह अपने पुरुषार्थ को भी छोड़ देगा जिसके उसके लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि आध्यात्मिक पथ को छुरे की धार पर चलने के समान दुष्कर कार्य बताते थे। अतः अनधिकारी को यह परम् वचन देने पर तो उसका सारा संतुलन ही बिगड़ सकता है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि गीता अपने इस परम् वचन के द्वारा पूर्व वर्णित सभी योग पद्धतियों की उपेक्षा नहीं कर रही है।
तब फिर आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे सभी रहस्यों में भी सर्वगुह्यतम बना देता है क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि को इन श्लोकों की भाषा में तो कोई रहस्यमय सूत्र प्रतीत नहीं होता। परंतु साथ ही यह भी निश्चित है कि गीता अनावश्यक रूप से किसी विशेषण का प्रयोग नहीं करती। यदि वह इसे सर्वगुह्यतमं बताती है तो अवश्य ही इसका वैसा स्वरूप है। अतः इसमें यह चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर इस कथन में ऐसी क्या विलक्षणता है और इसके निहितार्थ क्या हैं।
गीता शुरू से अंत तक जिन चीजों पर बल देती आ रही है वे हैं – योग की एक महान् और सुनिर्मित साधना-प्रणाली, एक व्यापक और सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति, स्वभाव और स्वधर्म, जीवन का सात्त्विक विधान जो मनुष्य को एक आत्म-अतिक्रमणकारी उन्नयन के द्वारा अपने घेरे से बाहर निकालकर एक अत्यंत सुविशाल, यहाँ तक कि इस उच्चतम गुण की सीमा के भी परे ऊँचे उठे हुए अमर अस्तित्व के मुक्त आध्यात्मिक धर्म की ओर ले जाता है, पूर्णता प्राप्त करने के अनेक नियम, साधन और अनिवार्य स्थितियाँ, और (इन सब पर जोर दे चुके होने के बाद) अब गीता एकाएक अपनी ही संरचना को तोड़कर उससे बाहर निकलती प्रतीत होती है और मानव आत्मा से कहती है, "सब धर्मों का परित्याग कर दे, अपने-आप को एकमात्र भगवान् के प्रति, अपने ऊपर, चारों ओर और अन्दर रहने वाले परमेश्वर के प्रति अर्पण कर दे : तुझे केवल यही करने की आवश्यकता है, यही सत्यतम और महत्तम पथ है, यही वास्तविक मुक्ति है।" कुरुक्षेत्र के दिव्य सारथि और दिव्य गुरु के रूप में सर्वलोक-महेश्वर ने मनुष्य के समक्ष ईश्वर, पुरुष और आत्मा की भव्य यथार्थताओं अथवा सत्यों को, इस जटिल जगत् की प्रकृति और परमात्मा के साथ मनुष्य के मन, प्राण, हृदय और इंद्रियों के संबंध को और उस विजयी साधन को प्रकाशित कर दिया है जिसके द्वारा वह अपने ही आध्यात्मिक साधनाभ्यास और पुरुषार्थ के बल पर मृत्युशीलता से अमरता में और अपने सीमाबद्ध मानसिक जीवन से अपने असीम आध्यात्मिक जीवन में उठ सकता है। और अब मनुष्य में तथा सभी वस्तुओं के अन्दर विद्यमान आत्मा और भगवान् के रूप में बोलते हुए वे उससे कहते हैं, "यदि तू मेरे प्रति पूर्ण समर्पण कर सके, अपने अन्दर तथा सब भूतों के अन्दर अवस्थित आत्मा और परमेश्वर पर ही निर्भर रह सके और एकमात्र उन्हीं के मार्गदर्शन पर भरोसा रख सके, तो अंत में इस सब वैयक्तिक पुरुषार्थ और आत्म-साधना की आवश्यकता नहीं रहेगी, नियम-धर्म के समस्त अनुसरण एवं सीमाबंधन को अंततः बाधक और भारस्वरूप समझकर त्यागा जा सकता है। अपना संपूर्ण मन मेरी ओर फेर दे और इसे मेरे तथा मेरी उपस्थिति के विचार से भर दे। अपने संपूर्ण हृदय को मेरी ओर लगा दे, अपने प्रत्येक कर्म को, वह चाहे जो भी क्यों न हो, मेरे प्रति यज्ञ और भेंट के रूप में परिणत कर। ऐसा कर लेने पर, तुम्हारे जीवन, अंतरात्मा और कर्म का मुझे मेरी अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने दे; अपने मन, हृदय, जीवन और कर्म-कलाप के साथ होनेवाले मेरे व्यवहारों से दुःखित या विभ्रांत मत हो और न इसलिए ही व्यथित हो कि ये उन नियमों और धर्मों का पालन नहीं करते प्रतीत होते जिन्हें मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि और इच्छाशक्ति के मार्गदर्शन के लिए अपने ऊपर लादता है। मेरी कार्य-शैलियाँ एक पूर्ण ज्ञान, शक्ति एवं प्रेम की कार्य-शैलियाँ हैं जो सभी वस्तुओं को जानता है और सर्वांगपूर्ण चरम परिणाम को लक्ष्य में रखकर अपनी सब गतियों को संयुक्त करता है; क्योंकि वह एक समग्र पूर्णता के अनेक सूत्रों को परिष्कृत करता और आपस में गूँथता है। मैं यहाँ युद्ध के रथ में तेरे साथ अवस्थित हूँ, तेरे अंदर और बाहर जगत् के अधीश्वर के रूप में प्रकटित हूँ, और मैं इस चरम आश्वासन एवं अमोघ प्रतिज्ञा को पुनः दुहराता हूँ कि मैं तुझे समस्त दुःख और पाप से उबारकर इनके परे अपनी ओर ले चलूँगा। चाहे जो भी कठिनाइयाँ और दुविधाएँ क्यों न उत्पन्न हों, इस बारे में आश्वस्त रह कि मैं तुझे विश्व-सत्ता के अंदर पूर्ण जीवन की ओर तथा विश्वातीत आत्मा के अंदर अमर स्थिति की ओर ले चल रहा हूँ।"
यदि हम गीता के परम् रहस्य की उत्कृष्टता तथा उसकी परम् महत्ता का कुछ आभास प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए आवश्यक है कि दिखने में जो बिल्कुल सहज से श्लोक प्रतीत होते हैं उनकी वास्तविक गंभीरता को समझने का प्रयास करें जिन्हें प्रदान करने के लिए सारी गीता का विकास किया गया है। गीता का आरंभ होता है दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक से जब अर्जुन कहता है कि 'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' अर्थात् 'मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, मुझे ज्ञानोद्दीप्त कीजिये।' और वह अपनी शिक्षा की समाप्ति पूर्ण समर्पण के स्वर के साथ करती है। समर्पण ही साधना का प्रथम स्वर है। योगी श्रीकृष्णप्रेम कहते हैं कि समर्पण "बिना किसी दावे के, बिना किसी माँग के और अपने-आप को दे देने की अनुमति लाभ करने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य किसी इच्छा के बिना अपने-आप को चरम और पूर्ण रूप से श्रीकृष्ण को सौंप देना है। वे सभी कार्य जो इस दान में सहायता करते हैं या इसके प्रतीक हैं वे सब साधना हैं। इस दान के परिणामस्वरूप सभी कार्य उनकी दिव्य लीला के अंग हैं।" (योगी श्रीकृष्णप्रेम, १६५) परंतु आखिर गीता के इन श्लोकों में उत्तमम् रहस्यं की क्या बात है क्योंकि प्रायः अधिकांश योग पद्धतियाँ समर्पण के ऊपर ही बल देती हैं। और फिर यदि भगवान् को समर्पण का ही उपदेश करना था तो दूसरे अध्याय में ही वे ऐसा कर सकते थे। यही नहीं, अनेक स्थानों पर श्रीकृष्ण ने 'सर्वभावेन भारत' आदि पदों से इस समर्पण की ओर संकेत किया भी है। वे यह भी कह चुके हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, यक्षों, गंधर्वी आदि को पूजने वाले उन-उन के पास जाते हैं। और 'मुझे' पूजने वाले मेरे पास आते हैं। वहीं एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं कि जो ऐसा जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। अतः इस ओर भगवान् बार-बार संकेत करते ही रहे हैं। अतः यदि भगवान् स्वयं इसे सर्वगुह्यतम रहस्य न कहते तो इस वचन की प्रतीत होती सादगी के कारण कदाचित् हम इसे चूक ही जाते। इसके विषय में किसी का दृष्टिकोण यह हो सकता है कि गीता यहाँ समर्पण की एक ऐसी अवस्था का संकेत करती प्रतीत होती है जहाँ किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत साधना या पुरुषार्थ आदि की कोई बात नहीं है। इसे वह एक ऐसी स्थिति के रूप में देख सकता है जहाँ स्वयं भगवान् हमारे अंदर आनंद लेने लगते हैं और हमारी सत्ता को स्वयं के उपयोग में लेने लगते हैं। उस स्थिति में आवश्यक नहीं है कि स्वयं उस व्यक्ति को भी उस क्रिया का कुछ पता हो। हो सकता है भगवान् उसके द्वारा जिस प्रकार अभिव्यक्त होते हों, उसके मन, प्राण, शरीर को जिस प्रकार जिस कार्य या जिस अभिव्यक्ति के लिए उपयोग में लेते हों उसे देखकर स्वयं वह व्यक्ति गहरे आश्चर्य का भाव रखता हो क्योंकि वह क्रिया उसके किन्हीं भी मानदंडों से सर्वथा परे होती है जिसका अपना ही विधान होता है। उस स्थिति में स्वयं भगवान् ही उसके द्वारा बोल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, कर्म का संचालन कर रहे होते हैं। और जिस मुक्त रूप से वे उसके द्वारा क्रिया करते हैं, संभव है उसे देखकर स्वयं वह व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हो या विचलित हो। परंतु यदि हम इस रहस्य का इस रूप में अर्थ लगाएँ तो इसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि गीता में यहाँ भगवान् ऐसा नहीं कह रहे कि यह स्वतः ही प्राप्त होने वाली स्थिति है अपितु वे अर्जुन को ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। वे कहते हैं 'मन्मना भव' अर्थात् मेरे मन वाला बन। इसके आगे वे कहते हैं मुझे नमस्कार कर, सभी धर्मों का परित्याग कर। अतः यदि हम यह दृष्टिकोण रखें कि यह अवस्था स्वतः ही आ जाती है तो हमें गीता के वचनों पर भी ध्यान देना चाहिये कि वह अर्जुन से ऐसा सब करने को कह रही है। इसी संदर्भ में हम पाते हैं कि पांडिचेरी स्थित आश्रम में श्रीमाताजी व श्रीअरविन्द के प्रति बहुतों की यह धारणा थी कि चूंकि वे तो अवतार हैं और मानवीय चेतना से बहुत परे हैं इसलिए उन्हें मानवीय समस्याओं को नहीं झेलना पड़ता अतः उनके लिए उन समस्याओं से ऊपर उठने का उपदेश करना आसान है। परंतु सामान्य मनुष्यों को तो सभी समस्याओं को झेलना पड़ता है। इसके उत्तर में श्रीअरविन्द जो कहते हैं वह बहुत ही प्रकाशक है। वे कहते हैं, "तुम कहते हो कि यह तरीका (उचित मनोभाव बनाए रखना) तुम्हारे लिए या तुम्हारे जैसों के लिए बहुत कठिन है और केवल मेरे या श्रीमाँ जैसे 'अवतार' ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। यह एक विचित्र गलत धारणा है, क्योंकि कठिन नहीं उल्टे यह तो सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे सीधा तरीका है और कोई भी इसे कर सकता है यदि वह अपने मन को और प्राण को शांत कर ले, तुमसे दसवें हिस्से की योग्यता वाले भी इसे कर सकते हैं। इससे भिन्न जो चिंता और तनाव और कठोर उद्यम का तरीका है वह कठिन है और उसमें तपस्या की महत् शक्ति की आवश्यकता होती है। जहाँ तक श्रीमाँ की और स्वयं मेरी बात है, हमें तो सभी तरीकों को प्रयोग कर देखना पड़ा है, सभी पद्धतियों का अनुसरण करके देखना पड़ा है, समस्याओं के पहाड़ों को पार करना पड़ा है, तुमने या आश्रम में अन्य किसी ने या आश्रम से बाहर किसी ने जितना वहन किया होगा उससे कहीं अधिक भारी बोझ, कहीं अधिक मुश्किल परिस्थतियाँ वहन करनी पड़ी हैं, कहीं अधिक संग्राम लड़ने पड़े हैं, और कहीं अधिक घावों को सहन करना पड़ा है, अभेद्य दलदल और मरुभूमि और जंगल से चीर कर मार्ग बनाने पड़े हैं, विरोधी समुदायों को जीतना पड़ा है, एक ऐसा काम जिसके बारे में मैं सुनिश्चित हूँ कि हमसे पहले किसी और को नहीं करना पड़ा है। क्योंकि जैसा कार्य हमने लिया है वैसे कार्य में 'मार्ग के नेता' को न केवल भगवान् को नीचे उतार लाना तथा उनका प्रतिनिधित्व करना और उन्हें मूर्त रूप ही प्रदान करना होता, अपितु मानवजाति के आरोही तत्त्व का भी प्रतिनिधित्व करना होता है और मानवता के बोझ को पूरी तरह वहन करना होता है और केवल एक क्रोड़ा या लीला के रूप में ही नहीं अपितु बिल्कुल विकट रूप से पथ पर संभव समस्त बाधा, कठिनाई, विरोध से चकित और बाधित होते हुए और केवल धीरे-धीरे विजयी होते श्रम के रूप में अनुभव करना होता है।" (CWSA 32, 94)
यही नहीं, श्रीअरविन्द के बहुत से अन्य पत्रों से, उनकी अन्य कृतियों में आए अनेक संदर्भों से तथा उनके 'रिकॉर्ड ऑफ योग' ग्रंथों से स्पष्ट रूप से यह पता लगता है कि श्रीअरविन्द ने कैसी अकल्पनीय तकलीफों को सहन किया, कैसा अभूतपूर्व श्रम किया और योग संबंधी सभी संभव तरीकों की किस प्रकार जाँच-परख करके उन्हें अनुभवसिद्ध किया। श्रीअरविन्द ने अपनी साधना को आंरभ से ही समर्पण पर आधारित किया। अपने गुरु, विष्णु भास्कर लेले के विषय में श्रीअरविन्द बताते हैं कि भले ही लेले बुद्धि, शिक्षा और योग्यता में स्वयं उनकी तुलना में अत्यंत अवर थे परंतु फिर भी उनके पीछे उन्होंने (श्रीअरविन्द ने) एक दिव्य शक्ति देखी जिसके कारण उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से उनके मार्गदर्शन के प्रति समर्पित कर दिया। स्वयं लेले उनके समर्पण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दूसरों को भी इसके विषय में बताया कि इतना पूर्ण, निर्विवाद और निःशेष समर्पण उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसी पूर्ण समर्पण के परिणामस्वरूप श्रीअरविन्द को श्रृंखलागत रूप से अनेकों ऐसे रूपांतरकारी अनुभव हुए जो कि स्वयं लेले के अनुभव से परे थे। इस कारण लेले ने स्वयं अपने मार्गदर्शन से मुक्त करते हुए श्रीअरविन्द को उनके अपने भीतरी दिव्य मार्गदर्शक का ही अनुसरण करने को कहा। और श्रीअरविन्द ने सदा यही किया भी। परंतु इस समर्पण को हम श्रीअरविन्द की ऊपर कही बात से जोड़ कर देखें कि उन्हें जीवन में जिन संकटों से गुजरना पड़ा वैसे संकट कदाचित् ही किसी को सहन करने पड़े होंगे तब इससे यह कुछ-कुछ स्पष्ट होता है कि जिस समर्पण की बात की जा रही है वह बड़ी ही गंभीर चीज है। स्वयं श्रीमाताजी की कृतियों से तथा उनकी वार्ताओं से उजागर होता है कि पाँच वर्ष की आयु में भी मनुष्यता से ऊपर होने पर भी तथा अनेकों जन्मों से पूर्व में तैयार किया गया अतिविशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त होने पर भी उन्हें जिन भीषण संघर्षों से गुजरना पड़ा उन्हें तो केवल स्वयं माँ जगदंबा ही सहन कर सकती थीं अन्य किसी मानव में तो वैसी पीड़ा सहन करने का कोई सामर्थ्य नहीं होता। श्रीमाताजी के समर्पण के विषय में श्रीअरविन्द कहते हैं कि श्रीमाँ ने स्वयं को अपनी भौतिक सत्ता तक में भी पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित कर दिया था और अपने आप को एक कोरे कागज की भाँति उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया था। अमल किरण की पुस्तक 'आवर लाइट एंड डिलाइट' में हमें यह संदर्भ मिलता है जहाँ श्रीअरविन्द कहते हैं कि, "जब मिरा ने अपने आप को मुझे समर्पित किया उससे पहले 'समर्पण' के अर्थ का मुझे कभी भी पता नहीं था।" इसी संदर्भ में जब उनसे पूछा गया कि श्रीमाताजी को प्रथम बार देखकर उन्हें क्या महसूस हुआ, तो इसके उत्तर में वे आगे कहते हैं कि, "पहली बार मुझे पता चला कि भौतिक कोशिका मात्र तक भी पूर्ण समर्पण मानवीय रूप से संभव था; जब श्रीमाँ आई और मुझे प्रणाम किया तब उस पूर्ण निःशेष समर्पण को मैंने क्रियान्वित होते देखा।" (पृष्ठ ७-८)
इन सब बातों पर विचार करने से हमें यह आभास होने लगता है कि गीता की जो उक्ति हमें यों सहज प्रतीत होती है उसके वास्तविक अर्थ बहुत ही गंभीर हैं। साथ ही गीता के संदर्भ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि समर्पण करने का अर्थ निष्क्रिय या निश्चेष्ट हो जाना भी नहीं है, जैसा कि समर्पण शब्द से बहुत बार अर्थ लगाया जाता है, क्योंकि इसके बाद तो अर्जुन को अभी भीषण युद्ध में प्रवृत्त होना बाकी है। अतः यह रहस्य कोई सीधी रेखा नहीं है अपितु बहुत ही सूक्ष्म और बहुआयामी चीज है।
गीता के इस परम् वचन को देखने के अनेक संभव दृष्टिकोण हो सकते हैं। अतः आगे चलने से पहले उन दृष्टिकोणों में से कुछ को चर्चा करना और उन पर विचार करना लाभप्रद होगा। एक दृष्टिकोण तो यह हो सकता है कि सामान्यतः जब हम समर्पण की बात करते हैं तो ऐसा मात्र कहने के लिए होता है जबकि व्यवहार में व्यक्ति समर्पण की आड़ में आवश्यक श्रम से बचना चाहता है और यह चाहता है कि सभी कुछ भगवान् ही कर दें ताकि उसे स्वयं कुछ न करना पड़े। अधिकांशतः व्यक्ति समर्पण का केवल नाम ही लेता है जबकि वास्तव में तो वह अपने अहं की तथा अपनी सत्ता के निम्न भागों की तुष्टि में ही लगा रहता है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति स्वयं भी इस बारे में पूर्णतः सचेतन हो कि वह कहता एक चीज है और व्यवहार में करता कुछ और है क्योंकि हमारे मन और प्राण हमारे अपने कृत्यों के लिए इस प्रकार के लुभावने स्पष्टीकरण देते हैं कि व्यक्ति को वास्तव में ही लगता है कि उसने सच्चा समर्पण कर दिया है और स्वयं भगवान् ही उसके समर्पण को स्वीकार कर उसके द्वारा क्रिया कर रहे हैं। अतः इस प्रकार का समर्पण केवल कहने भर को ही समर्पण होता है जबकि वास्तव में इसका समर्पण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता और समर्पण की आड़ में अधिकांशतः केवल धोखा ही होता है। यहाँ जिस समर्पण की बात की जा रही है वह लगता तो सहज है परंतु वास्तव में व्यवहार में उसे कर पाना अत्यंत दुष्कर है।
इसे देखने का एक अन्य दृष्टिकोण भी हो सकता है। अब तक गीता ने अनेकों योग-पद्धतियों की बातें की हैं, कर्मों का, ज्ञान का और भक्ति का समन्वय साधा है, अनेकों धर्मों की बातें की हैं। यदि कुछ गहरे दृष्टिकोण से देखें तो विकास की किसी अवस्था पर आकर व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि उसे होने वाले सभी अनुभव उसकी सीमित मानसिक, प्राणिक और भौतिक संरचना के दायरे में ही होते हैं जो कि परम् सत्य के अनुपात में बहुत ही संकीर्ण होते हैं और साथ ही उसे कुछ-कुछ यह अनुभव हो जाता है कि उसकी संरचना के अनुसार उसके मन का किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों, आधारों या धर्मों पर आग्रह रहता है। इसलिए जब तक यह संकीर्णता रहती है तब तक व्यक्ति उन्मुक्त रूप से उस परम् सत्ता में निवास नहीं कर सकता। अतः जब गीता सभी धर्मों के परित्याग करने की बात करती है तब उससे यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि यह उस संकीर्ण संरचना विशेष के त्याग के लिए कह रही है। और भले ही यह परित्याग सुनने में सहज प्रतीत होता हो परंतु इसकी चरितार्थता अत्यंत जटिल और कठिन है। और जब व्यक्ति यह परित्याग कर सके तब उसकी सत्ता को भगवान् मुक्त रूप से अपनी क्रिया का यंत्र बना सकते हैं। साथ ही यह मार्ग सभी के लिए नहीं अपितु केवल चयनित आत्माओं के लिए ही होता है। श्रीअरविन्द कहते हैं कि यह रहस्य श्रीगुरु अर्जुन को प्रकट करते हैं, "क्योंकि वह उनकी चुनी हुई और प्रिय आत्मा है, उनका 'इष्ट' है। क्योंकि स्पष्ट हो, जैसा कि उपनिषद् पहले ही घोषित कर चुका है, अपने वास्तविक स्वरूप को, 'तनुं स्वाम्', प्रकाशित करने के लिए परमात्मा के द्वारा चुना हुआ कोई विरला जीव ही इस रहस्य में प्रवेश पा सकता है, क्योंकि केवल वही हृदय, मन और प्राण में परमेश्वर के इतना पर्याप्त निकट होता है कि वह अपनी सारी सत्ता में उन्हें सच्चे रूप में प्रत्युत्तर दे सकता है अथवा उनके अनुकूल हो सकता है तथा उसे अपना जीवंत अभ्यास बना सकता है।"
जिस गुह्य तत्त्व, 'गुह्यम्', को समस्त गंभीर अध्यात्मज्ञान हमारे समक्ष प्रकाशित करता है, जो विविध शिक्षाओं में प्रतिबिंबित दिखाई देता है तथा आत्मा की अनुभूति के द्वारा प्रमाणसिद्ध होता है वह, गीता की दृष्टि में, हमारे अंदर प्रच्छन्न अध्यात्म-सत्ता का रहस्य है, मन और बाह्य प्रकृति उस सत्ता की अभिव्यक्तियाँ या रूप मात्र हैं। वह गुह्य तत्त्व पुरुष और प्रकृति के नित्य संबंधों का रहस्य है, उन अंतर्यामी ईश्वर का रहस्य है जो समस्त जगत् के प्रभु हैं और इसके रूपों तथा क्रियाओं के अंदर हमसे छुपे हुए हैं। ये सत्य हैं जिन्हें अनेक तरीकों से वेदांत, सांख्य और योग द्वारा उपदेशित किया गया है और गीता के शुरू के अध्यायों में समन्वित किया गया है। अपने सब भिन्न बाह्य भेदों या प्रतीतियों के होते हुए भी ये एक ही सत्य हैं और योग के सब विभिन्न मार्ग आध्यात्मिक साधना के विविध साधन हैं जिनके द्वारा हमारे अशांत मन तथा अंधे हुए प्राण को शांत-स्थिर किया जाता है और इन बहुपक्षीय एकमेव की ओर मोड़ दिया जाता है और आत्मा तथा ईश्वर के निगूढ़ सत्य को हमारे लिए इतना वास्तविक एवं अंतरंग बना दिया जाता है कि या तो हम उसमें सचेतन रूप से जीवन यापन कर सकते एवं निवास कर सकते हैं अथवा हम अपनी पृथक् सत्ता को सनातन में खो दे सकते हैं और तब हम पहले की तरह मानसिक अज्ञान के जरा भी वशीभूत नहीं रहते।
यह सांख्ययोगियों या ज्ञानमार्गियों का मार्ग है जो ऐसा जानकर कि गुण गुणों के अंदर क्रिया कर रहे हैं संसार के प्रति शांत-स्थिर या उदासीन भाव अपनाकर अपनी इंद्रियों को संयमित और शांत करके, अपने मन, प्राण की वृत्तियों का निरोध अथवा संयम करके, साक्षी भाव अपनाकर अक्षर ब्रह्म अथवा अपनी अध्यात्म-सत्ता की ओर अपने ध्यान को लगाकर विश्व प्रपंच से अपने आप को बिलग कर उसी स्थिति में अपने आप को अवस्थित करने का प्रयास करते हैं। श्री अरविन्द कहते हैं कि यह गुह्य रहस्य है। रहस्य इसलिए है क्योंकि संसार में रहते हुए हम बाह्य प्रतीतियों से इतने अभिभूत रहते हैं कि सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता कि यह सारा दृश्य प्रपंच है और इसके पीछे एक गूढ़ सत्य या परमात्म सत्ता है जो इस सारे दृश्य प्रपंच को अनुप्राणित करती है। भले ही हम पुस्तकों आदि के माध्यम से यह पढ़ या सुन लें कि इन सब
प्रतीतियों के पीछे दिव्य शक्ति कार्य करती है, कि सारा संसार आत्मा की शक्ति के द्वारा चालित होता है, परंतु फिर भी हमारी श्रद्धा हमारे इंद्रिय-विषयों पर आधारित और उनमें इतनी अधिक संलग्न और लिप्त होती है कि उसे इस सत्य पर विश्वास ही नहीं आ पाता। अतः भीतर इस सत्य के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा का जागृत होना भी एक बड़ा भारी पग है क्योंकि एक बार यदि यह विश्वास जागृत हो जाए तो व्यक्ति सक्रिय रूप से उस दिशा में प्रयत्न करता है, अपने चित्त की वृत्तियों पर, मन, प्राण की इच्छाओं, लालसाओं, कामनाओं, पूर्वधारणाओं, पूर्वाग्रहों आदि का साक्षित्व करता है और उन्हें संयमित करने का पूरा प्रयास करता है। और जब मन और प्राण के उद्वेग कुछ शांत होते हैं तब व्यक्ति को इस दृश्य प्रपंच से महत्तर सत्ता का कुछ-कुछ आभास होने लगता है जिसमें कि शाश्वतता है, अक्षरत्व है। यह एक ऐसा अनुभव है जो बहुत ही महान् है और अनेकों लोगों को यह अनुभव हुआ भी है। एक बार यह अनुभव होने पर व्यक्ति एक भिन्न पायदान पर आरोहित हो जाता है। हालाँकि इसके बाद भी अनंत यात्रा अभी बाकी रहती है, परंतु फिर भी इससे व्यक्ति घोर क्षरत्व से कुछ मुक्त हो जाता है। भावी भवितव्यताओं के दृष्टिकोण से तो यह अनुभव और यह अवस्था गुह्य तत्त्व में एक प्रवेश मात्र है। परंतु यदि हमारे वर्तमान जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अनुभव एक बहुत ही महान् पग है। और बहुत सी योग पद्धतियों में तो इसे बहुत ही उच्च स्थिति मानते हैं, कुछ में तो इसे लगभग अंतिम स्थिति ही मानते हैं जिसमें कि व्यक्ति का ब्रह्म-निर्वाण साधित हो जाता है या फिर जो ब्रह्म में लीन हो जाता है और केवल साक्षी भाव से ही इस पार्थिव जीवन को व्यतीत करता है। परंतु चूँकि हमारे वर्तमान बद्ध पार्थिव जीवन के लिए तो यह आभास या अनुभव कर पाना भी एक महान् पग है कि इस दृश्य प्रपंच के पीछे किसी महत्तर सत्ता की विद्यमानता है, इसीलिए इसे गुह्य ज्ञान कहा गया है। और जब व्यक्ति को यह गुह्य ज्ञान हो जाता है तब वह पाता है कि पार्थिव अभिव्यक्ति में जो चीजें हमें गोचर होती हैं वे तो मानो उन महत्तर जगतों के वैसे ही विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं जैसे विकृत प्रतिबिंब किसी गंदे पानी में बना करते हैं। परंतु गीता की विलक्षणता यह है कि अन्य योगों से अलग गीता के अनुसार यह ब्राह्मी स्थिति शरीर में रहते हुए भी प्राप्त की जा सकती है। गीता ने सबसे पहले इसी अक्षर ब्रह्म को स्थापित करके अपनी शिक्षा का आरंभ किया था। गीता इस रहस्य के परे एक गुह्यतर तत्त्व की बात करती है।
गीता द्वारा विकसित इससे भी अधिक गुह्य तत्त्व, 'गुह्यतरम्', उन भगवान् पुरुषोत्तम का गंभीर समन्वयकारी सत्य है, जो एक ही साथ आत्मा भी हैं और पुरुष भी, परब्रह्म भी हैं और एकमेव, अंतरंग, रहस्यमय, अनिर्वचनीय परमेश्वर भी। यह गुह्यतर तत्त्व हमारे चिंतन को चरम ज्ञान के लिए एक विशालतर तथा अधिक गहरे रूप से समझने वाला आधार प्रदान करता है, और साथ ही हमारी आध्यात्मिक अनुभूति को यह एक महत्तर तथा अधिक पूर्ण रूप से समन्वयकारी तथा व्यापक योग प्रदान करता है। यह गंभीरतर रहस्य परा आध्यात्मिक प्रकृति और जीव के रहस्य पर आधारित है, जीव उस शाश्वत तथा इस व्यक्त प्रकृति में भगवान् का सनातन अंश है और अपनी अक्षर आत्म-सत्ता में उनके साथ आत्मतः और मूलतः एक है। यह गंभीरतर ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा किये गए परात्पर तत्त्व और इहलोक के बीच आरंभिक भेद से परे निकल जाता है। क्योंकि, जगतों के परे जो परात्पर है वह साथ-ही-साथ वासुदेव भी है जो सब लोकों की सभी वस्तुएँ बना हुआ है, वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में अवस्थित ईश्वर तथा सर्वभूतों का आत्मा है और अपनी प्रकृति में उसने जो कोई भी चीज प्रकट की है उसका उद्गम एवं दिव्य अर्थ है। वह अपनी विभूतियों में प्रकट हुआ है, वह कालगत पुरुष है जो जगत् के क्रिया-व्यापार को चलायमान करता है, वह समस्त ज्ञान का सूर्य, जीव का प्रेमी और प्रियतम, समस्त कर्मों और यज्ञ का स्वामी है। इस गंभीरतर, सत्यतर, गुह्यतर रहस्य की ओर अंतरतम उद्घाटन का फल होता है गीता का समग्र ज्ञान, समग्र कर्म और समग्र भक्ति का योग। यह एक ही साथ आध्यात्मिक विश्वमयता और मुक्त तथा पूर्णताप्राप्त आध्यात्मिक व्यटिभाव का अनुभव है, यह परमेश्वर के साथ पूर्ण रूप से एक होने का अनुभव है और साथ ही उन्हें जीव की अमरता का आधार तथा जगत् और देह में हमारे मुक्त कर्म का आश्रय एवं शक्ति जानते हुए उनके अंदर पूर्ण रूप से निवास करने का अनुभव भी है।
यह अनुभव गुह्य से भी गुह्यतर है क्योंकि यह एक अधिक महत्तर सत्य है। इससे पूर्व का जो अनुभव था उसमें व्यक्ति को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। उसे अपने आप पर भारी संयम रखते हुए सभी चीजों से निर्लिप्त रहना पड़ता है अन्यथा किसी भी चीज में लिप्त होकर उसकी अपने पथ से च्युत होने की, योगभ्रष्ट होने की आशंका बनी रहती है। उस स्थिति को बनाए रखने के लिए उसे अधिकांश समय एक प्रकार की समाधि अवस्था में रहना होता है जहाँ केवल शरीर को बनाए रखने के लिए मूलभूत क्रियाओं को ही किया जाता है और अन्य सभी प्रकार के कर्मों को लगभग बंद ही कर दिया जाता है क्योंकि कर्म बंधनस्वरूप प्रतीत होते हैं जो कि व्यक्ति को पुनः इस प्रपंच से बाँध देते हैं। इसलिए भले ही सामान्य पार्थिव जीवन के दृष्टिकोण से यह स्थिति बड़ी ही महान् प्रतीत हो परंतु फिर भी स्पष्ट ही है कि यह किसी प्रकार के पूर्णत्व की स्थिति नहीं हो सकती। इससे आगे भगवान् एक ऐसी स्थिति का वर्णन करते हैं जो क्षर और अक्षर दोनों से ही परे है। हालाँकि आरंभ में तो वे 'अहं', 'माम्' आदि पदों से अपनी सत्ता को प्रतिपादित करते हैं परंतु वास्तव में यह प्रकट नहीं करते कि वे हैं कौन। पंद्रहवें अध्याय में आकर ही स्पष्ट रूप से वे अपनी सत्ता को प्रकट करते हुए अक्षर और क्षर से परे पुरुषोत्तम के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करते हैं। जब उन्हें पुरुष और प्रकृति के भेद से देखा जाता है तब वे पुरुषोत्तम हैं, जब उन्हें जीव और आत्मा के रूप में देखा जाता है तब वे परमात्मा हैं, जब ईश्वर और उनकी शक्ति के रूप में देखा जाता है तब वे परमेश्वर हैं और जब उन्हें ब्रह्म और सृष्टि या माया के रूप में देखा जाए तो वे परंब्रह्म हैं। अतः स्वभाव और स्वधर्म की चर्चा में भगवान् कहते हैं कि व्यक्ति को पहले सतही भाव से अपने आंतरिक स्वभाव की ओर जाना होता है और वहाँ से फिर भगवान् के भाव में जाना होता है, 'मद्भावमागता'। जब व्यक्ति भगवान् के भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है तब वह क्षर और अक्षर दोनों से ही परे पहुँच जाता है। इस संदर्भ में स्वयं अपना उदाहरण देते हुए भगवान् बताते हैं कि किस प्रकार वे स्वयं सभी कर्मों को करते हुए भी उनसे बद्ध नहीं होते अपितु समस्त कर्मों के अधीश्वर रहते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम भाव ही ऐसा भाव है जिसमें व्यक्ति क्षर और अक्षर दोनों ही भावों में विजयी रूप से निवास और क्रिया करते हुए भी उनसे सीमित या बद्ध नहीं होता अपितु उनसे परे पुरुषोत्तम के भाव में प्रतिष्ठित हो सकता है। यही सच्ची पूर्णता है। इसमें फिर कोई कर्म बंधनकारी नहीं होते अपितु समस्त कर्म मात्र उसके संकल्प से ही होते हैं। इसीलिए वह घोर से घोर कर्मों को करते हुए भी सर्वथा उनसे परे अकर्ता बना रहता है। इसी पुरुषोत्तम की ओर गति करने के लिए गीता पूर्ण भक्ति, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण कर्मों के समन्वय की बात करती है। इसके लिए व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार किसी भी एक से आरंभ कर सकता है और ज्यों-ज्यों वह मार्ग में विकसित होता जाता है त्यों-ही-त्यों अन्य दूसरे भी उसमें सम्मिलित होते जाते हैं क्योंकि कोई भी पूर्ण कर्म उस कर्म के विषय में ज्ञान हुए बिना और जिसके लिए कर्म किया जा रहा है उसके प्रति भाव हुए बिना संपन्न नहीं हो सकते। साथ ही, जब अपने प्रेमी के सत्स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति कर्म किये बिना रह ही नहीं सकता। तो इस प्रकार, व्यक्ति अपने स्वभाव अनुसार भले किसी भी एक से आरंभ करे परंतु पूर्णत्व लाने के लिए अन्य दूसरे अंग स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। पुरुषोत्तम की चेतना ही विजयी रूप से क्रिया करने का आधार हो सकता है और वही वह सच्ची स्थिति हो सकती है जिसमें व्यक्ति को सतर्क रूप से अपने चारों ओर किन्हीं संयमों या नियमों की बाड़ नहीं करनी पड़ती ताकि वह किसी भी प्रकार अपनी स्थिति को बनाए रख सके और उससे च्युत न हो जाए। जब तक व्यक्ति एक ऐसी अपूर्ण और संदिग्ध स्थिति में रहता है जहाँ प्रत्येग पग पर उसे सतर्क रहना पड़े और जीवन से सर्वथा निर्लिप्तता रखनी पड़े ताकि वह अपनी स्थिति से गिर नहीं जाए तब तक उसे इस जगत् को मिथ्या-माया मानना पड़ता है क्योंकि यदि वह ऐसा कोई कृत्रिम भेद न करे तो अपनो स्थिति को बनाए रखने का उसके पास कोई मनोवैज्ञानिक आधार ही नहीं बचेगा। इसीलिए उसे एक तीक्ष्ण विभेद करना पड़ता है और उसी के सहारे अपनी संदिग्ध स्थिति को बनाए रखना होता है। परंतु ऐसा करने से अभिव्यक्ति का सारा उद्देश्य ही निष्फल हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसमें तो सत्ता के विभिन्न भागों को शांत कर दिया जाता है परंतु ऐसा कर के उन्हें सभी प्रकार की अभिव्यक्ति के आनंद से ही वंचित कर दिया जाता है। जबकि इस दूसरी स्थिति में व्यक्ति को सर्वत्र जगदंबा की क्रिया दिखाई देती है और व्यक्ति स्वयं उसी का यंत्र होता है जिसमें उसके प्रत्येक भाग को अभिव्यक्ति का पूरा अवसर प्राप्त होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर किसी प्रकार की बाड़ नहीं करनी होती अपितु वह सभी कर्मों को जगदंबा की अभिव्यक्ति के रूप में करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में उसकी संपूर्ण सत्ता को अपनी पूर्ण चरितार्थता का आनंद प्राप्त होता है। परंतु बहुत सी योग प्रणालियों का मानना है कि स्वयं ईश्वर भी जब पृथ्वी पर अपनी क्रिया करते हैं तब उन्हें भी गुणों आदि से बद्ध होकर क्रिया करनी होती है और वे मुक्त नहीं होते। इसलिए उनके अनुसार कर्म मात्र ही बंधन का कारण है। परंतु इसी गुत्थी को सुलझाते हुए गीता सातवें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति के भेद को स्पष्ट करते हुए कहती है कि स्वयं पराप्रकृति ही जीव के रूप में प्रकट होती है। इसमें भी कुछ इसकी व्याख्या इस रूप में करते हैं कि पराप्रकृति जीव के रूप में सीमित हो जाती है। परंतु इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पराप्रकृति जीव बन कर भी केवल जीव भाव से बद्ध नहीं हो जाती अपितु वह तो जीव के अतिरिक्त भी जो कुछ है वह सभी कुछ बनी रहती है। मनुष्य की आत्मा ही वह कड़ी है जो परा और अपरा प्रकृति को जोड़ती है। इस तरह इस सूक्ष्म भेद को बताकर गीता यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार यह पराप्रकृति इस दृश्यमान अपरा प्रकृति में अपनी क्रिया करती है। और यही वह रहस्य है जो कि इस पार्थिव अभिव्यक्ति में दिव्य कर्मों को संभव बना देता है। अतः जब व्यक्ति अपने आप को उठाकर दिव्य चेतना के साथ संयुक्त कर देता है तब फिर वह चेतना उसके द्वारा अभिव्यक्त हो सकती है। और यही वास्तव में इस पार्थिव अभिव्यक्ति का सच्चा उद्देश्य है। अन्यथा इसका कोई कारण समझ नहीं आता कि परमेश्वर की ऐसी क्या बाध्यता हो सकती है जो अपने आप को किसी ऐसी बद्ध स्थिति में डाल दें जहाँ से किसी प्रकार बाहर निकलना ही उनका एकमात्र उद्देश्य हो। अतः उस स्थिति में पहुँचने का पूरा विधान गीता में वर्णित किया गया है जहाँ व्यक्ति मुक्त रूप से कर्म कर सकता है। परंतु यह सब विधान आदि की चर्चा कर चुके होने के बाद गीता इससे भी आगे निकल जाती है। वह कहती है कि अवश्य हो यह प्रतीति होती है कि भगवान् किन्हीं विधानों के द्वारा आत्मा को ऊर्ध्व- यह रोहित करते हैं परंतु वास्तव में तो जब परमात्मा स्वयं ही गति कर रहे हैं तो उसमें हमें किन्हीं भी विधानों की प्रतीति भले ही हो, परंतु चूंकि उनकी निज सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विधान लागू ही कैसे हो सकता है। इसीलिए सभी योगों का निरूपण करने के बाद गीता जानती है कि भले ही अपने आप में ये सभी योग-प्रणालियाँ कितनी भी ऊँची क्यों न हाँ, परंतु तो भी हैं मानसिक विधान ही, और परमात्मा ऐसे किन्हीं भी विधानों से सीमित नहीं हो सकते। अतः वह इन सभी विधानों को तोड़ कर अपना गुह्यतम वचन प्रदान करती है।
और अब आता है परम वचन तथा सबसे गुह्य तत्त्व, 'गुह्यतमम्', वह यह है कि परमात्मा एवं भगवान् 'अनंत' हैं जो धर्मों से मुक्त हैं, और यद्यपि वे स्थिर नियमों के अनुसार जगत् का परिचालन करते हैं और मनुष्य को उनके अज्ञान और ज्ञान, पाप और पुण्य, सत् और असत्, राग और द्वेष और उदासीनता, सुख और दुःख, हर्ष और शोक के धर्मों के द्वारा तथा इन द्वंद्वों के परित्याग के द्वारा, उसके भौतिक और प्राणिक, बौद्धिक, भाविक, नैतिक और आध्यात्मिक रूपों, नियमों एवं आदर्शों के द्वारा ले चलते हैं, तथापि परमात्मा तथा भगवान् इन सब चीजों से परे हैं, और यदि हम भी धर्मों के समस्त अवलंबन को त्याग सकें, इन मुक्त और सनातन परमात्मा के प्रति अपने को समर्पित कर सकें और अपने-आप को केवल इनकी ओर पूर्ण तथा अनन्य भाव से खुला रखने का ही ध्यान रखते हुए, अपने अंतःस्थ भगवान् की ज्योति, शक्ति और आनंद पर भरोसा रख सकें और भय तथा शोक न करते हुए, केवल उन्हीं का मार्गदर्शन स्वीकार कर सकें, तो यह सत्यतम और महत्तम मुक्ति है और इससे हमें अपनी सत्ता एवं प्रकृति की चरम और अटल पूर्णता प्राप्त होती है। यह है वह मार्ग जो परम आत्मा द्वारा चयनितों के लिए प्रदर्शित किया गया है, - केवल उन लोगों के लिए जिनमें भगवान् अधिकतम आनंद लेते हैं, क्योंकि वे लोग उनके निकटतम हैं एवं उनके साथ एकत्व लाभ करने के लिए सर्वाधिक योग्य हैं और, प्रकृति की उच्चतम शक्ति एवं क्रिया के साथ स्वतंत्रतापूर्वक सहमत तथा सुसंगत होते हुए, उन्हीं की भाँति आत्मा की चेतना के अंदर विश्वमय और अध्यात्मसत्ता के अंदर विश्वातीत बनने में सर्वाधिक समर्थ हैं।
क्योंकि, आध्यात्मिक विकास में एक समय ऐसा आता है जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हमारा समस्त पुरुषार्थ और कर्म हमारे अंदर और हमारे चारों ओर विद्यमान एक महत्तर उपस्थिति के शांत और गूढ़ आग्रह के प्रति हमारी मानसिक एवं प्राणिक प्रतिक्रियाएँ मात्र ही हैं। हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा समस्त योग, हमारी अभीप्सा और हमारा उद्यम एक बृहत्तर सत्य के अशुद्ध या अर्धसत्य रूप हैं, क्योंकि ये मन के संसगाँ, माँगों, पूर्व-निर्णयों, पक्षपातों द्वारा विकृत या कम-से-कम उनसे सीमाबद्ध होते हैं। हमारे विचार, अनुभव तथा प्रयास महत्तम चीजों की मानसिक प्रतिमूर्ति मात्र हैं जो कि हमारे अंदर स्थित उस शक्ति द्वारा अधिक पूर्ण, प्रत्यक्ष, स्वतंत्र एवं विशाल रूप से तथा वैश्विक एवं सनातन संकल्प के साथ अधिक समस्वरता से संपादित हो सकते हैं यदि हम अपने-आपको सर्वोच्च एवं परम् शक्ति एवं प्रज्ञा के हाथों में यंत्रवत् समर्पित कर सकें। वह शक्ति हमसे पृथक् नहीं है; वह हमारी अपनी ही आत्म-सत्ता है जो अन्य सब की आत्म-सत्ता के साथ एक है और साथ-ही-साथ एक विश्वातीत सत्ता और अंतरस्थ पुरुष भी है। हमारा जीवन, हमारा कर्म इस महत्तम सत्ता में समाहित होकर व्यक्तिगत रूप से हमारा अपना नहीं रहेगा, जैसा कि अब हमें मानसिक पार्थक्य में यह प्रतीत होता है। यह एक अनंतता एवं अंतरंग अनिर्वचनीय उपस्थिति की एक बृहत् गति होगा; वह हमारे अंदर इस गहन वैश्विक आत्मा एवं इस विश्वातीत पुरुष की एक सतत् स्वयं-स्फूर्त रचना एवं प्राकट्य होगा। गीता यह इंगित करती है कि ऐसा पूर्ण रूप से हो, इसके लिए समर्पण निःशेष रूप से होना होगा; हमारे योग, हमारे जीवन तथा अंतः-सत्ता की अवस्था का निर्धारण मुक्त रूप से इस जीवंत 'अनंत' के द्वारा होना होगा, न कि इस या उस धर्म या किसी भी धर्म के ऊपर हमारे मन के पूर्वाग्रह द्वारा। तब योग के दिव्य ईश्वर, 'योगेश्वरः कृष्णः' स्वयं हमारे योग को अपने हाथों में लेंगे और हमें हमारी उच्चतम संभव पूर्णता तक ऊपर उठा ले जाएँगे, किसी बाह्य या मानसिक आदर्श या बंधनकारी नियम की पूर्णता तक नहीं अपितु एक विशाल और व्यापक तथा मन के लिए अपरिमेय पूर्णता तक। वह एक ऐसी पूर्णता होगी जो सर्वदर्शी प्रज्ञा के द्वारा पहले तो निःसंदेह मानव स्वभाव के समग्र सत्य के अनुसार, किंतु बाद में उस महत्तर वस्तु के समग्र सत्य के अनुसार विकसित होगी जिसकी ओर हमारा स्वभाव उद्घाटित होगा, - (वह महत्तर वस्तु है) एक असीम, अमर, मुक्त तथा सर्वरूपांतरकारी आत्मा एवं शक्ति तथा एक दिव्य और अनंत प्रकृति की ज्योति और दीप्ति।
सब कुछ उस रूपांतरण के आवश्यक द्रव्य के रूप में समर्पित कर देना होगा। एक सर्वज्ञ चेतना हमारे ज्ञान और अज्ञान, हमारे सत्य और असत्य को अपने हाथ में लेकर उनके अपर्याप्त रूपों को दूर कर देगी, 'सर्वधर्मान् परित्यज्य', और सब कुछ को अपनी अनंत ज्योति में रूपांतरित कर देगी। एक सर्वसमर्थ शक्ति हमारे पुण्य और पाप, उचित और अनुचित, बल और दुर्बलता को अपने हाथ में लेकर उनके उलझे हुए रूपों को सुलझा देगी, 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' और उन सबको अपनी विश्वातीत पवित्रता एवं सार्वभौम शुभ एवं अमोघ शक्ति में रूपांतरित कर देगी। एक अनिर्वचनीय आनंद हमारे क्षुद्र हर्ष और शोक, हमारे संघर्षरत सुख और दुःख को अपने हाथ में लेकर उनके विसंगत एवं त्रुटिपूर्ण लयों को दूर कर देगा, 'सर्वधर्मान् परित्यज्य', और उन सब को अपने विश्वातीत एवं विश्वगत अकल्पनीय आनंद में रूपांतरित कर देगा। समस्त योग जो कुछ कर सकते हैं वह सब और उससे भी अधिक किया जाएगा; परंतु यह एक महत्तर दृष्टि से किया जाएगा, जो कुछ कोई मानव गुरु, संत या ज्ञानी प्रदान कर सके उसकी अपेक्षा कहीं अधिक महत्तर प्रज्ञा एवं सत्य के साथ किया जाएगा। जिस आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति तक यह परम् योग हमें ले जायेगा, वह जो कुछ इस संसार में है उस सब से ऊपर होगी और फिर भी इस जगत् या अन्य लोकों की सभी वस्तुओं को अपने अंदर समाविष्ट करेगी, परंतु बिना सीमित हुए व बिना बंधन के सभी का आध्यात्मिक रूपांतरण करते हुए 'सर्वधर्मान् परित्यज्य'। भगवान् का अनंत सत्, चेतना (चित्) एवं आनंद अपनी शांत निश्चल-नीरवता तथा उज्ज्वल, अपार क्रिया के साथ वहाँ होगा, वह उस स्थिति का तात्त्विक, आधारभूत और विश्वगत उपादान, साँचा एवं स्वरूप होगा। तब, अनंतता के उस साँचे में इस प्रकार प्रकट हुए भगवान् पहले की तरह अपनी योगमाया के द्वारा आच्छादित होकर नहीं, अपितु प्रत्यक्ष रूप से निवास करेंगे और जब-जब तथा जिस प्रकार वे चाहेंगे तब-तब तथा उस प्रकार वे हमारे अंदर अनंत के चाहे जो आकार गठित कर लेंगे और अपने आत्म-परिपूर्तिकारी संकल्प एवं अमर आनंद के अनुसार ज्ञान, विचार, प्रेम, आध्यात्मिक आनंद, शक्ति और कर्म के ज्योतिर्मय रूपों का निर्माण कर लेंगे। वहाँ मुक्त आत्मा एवं अप्रभावित प्रकृति पर कोई भी बंधनकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इस या उस निम्नतर धर्म के अंदर ऐसा दृढ़ीकरण होगा जिससे बाहर न निकला जा सके। क्योंकि, समस्त कर्म दिव्य स्वतंत्रता, 'सर्वधर्मान् परित्यज्य', में परमात्मा की शक्ति द्वारा ही संपन्न होगा। विश्वातीत आत्मा में, 'परम धाम' में अविचल निवास ही इस आध्यात्मिक स्थिति का आधार एवं आश्वासन होगा। विश्वसत्ता और सर्वभूतों के साथ एक घनिष्ठ बोधपूर्ण एकता ही, जो भेदमूलक मन की बुराई और दुःख-ताप से मुक्त पर सच्चे भेदों की ओर ज्ञानपूर्वक ध्यान देनेवाली होगी इस स्थिति की नियामक शक्ति होगी। एक अखंड आनंद, तथा वे जो कुछ भी हैं उस सबके साथ यहाँ सनातन जीव का एकत्व एवं सामंजस्य ही इस सर्वांगीण मुक्ति का फल होगा। हमारे मानव अस्तित्व की चकरा देनेवाली समस्याएँ, अर्जुन की समस्या जिनका एक तीव्र दृष्टांत है, अज्ञान के अंदर हमारे भेद-जनक व्यक्तित्व के द्वारा उत्पन्न होती हैं। यह योग चूंकि परमेश्वर तथा जगत्-जीवन के साथ मानव आत्मा का यथार्थ संबंध स्थापित करता है, हमारे कर्म को भगवान् का कर्म, उसे गठित एवं परिचालित करनेवाले ज्ञान एवं संकल्प को भगवान् का ज्ञान एवं संकल्प तथा हमारे जीवन को दिव्य आत्म-अभिव्यक्ति का एक गतिच्छंद बना देता है, इसलिए, यह उन समस्याओं का पूर्ण रूप से निराकरण करने का वास्तविक मार्ग है।
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ।। ६७।।
६७. तेरे द्वारा इस ज्ञान को उसे नहीं बताया जाना चाहिए जो तप से या भक्ति से विहीन है, और न ही उसे जिसे सुनने की इच्छा नहीं है अथवा जो मेरी निन्दा करता है और मुझे गौण समझता है।
य इमं परमं गुहां मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ।। ६८।।
६८. जो मनुष्य मुझ में परम् भक्ति रखकर इस परम् गोपनीय रहस्य को मेरे भक्तों के बीच में कहेगा वह निस्संदेह ही मुझे प्राप्त होगा।
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्विन्मे प्रियकृत्तमः ।
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ।। ६९।।
६९. उसकी अपेक्षा मेरा अतिशय प्रिय कर्म करनेवाला संपूर्ण मनुष्यों में दूसरा कोई भी नहीं होगा और पृथ्वी पर मुझे उससे अधिक प्रिय दूसरा नहीं होगा।
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः ।
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ।। ७०॥
७०. और जो मनुष्य हमारे इस पवित्र संवाद को अध्ययन करेगा उससे मैं ज्ञानयज्ञ के द्वारा अर्चित हूँगा, ऐसा मेरा मत है।
श्रद्धावाननसूयश्व शृणुयादपि यो नरः ।
सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ।। ७१।।
७१. जो मनुष्य श्रद्धा से पूर्ण और दोषदृष्टि से रहित होकर इसका श्रवण करेगा वह मुक्त होकर पुण्य कर्म करनेवाले मनुष्यों को प्राप्त होनेवाले श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेगा।
कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ।। ७२।।
७२. हे पार्थ! क्या इसे एकाग्र चित्त के साथ तेरे द्वारा सुना गया है? हे धनञ्जय! तेरा जो अज्ञानजन्य मोह था, क्या वह नष्ट हुआ है?
अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्या त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।। ७३।।
७३. अर्जुन ने कहाः हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मैं संशयरहित हुआ दृढ़स्थित हूँ। मैं आपके वचन के अनुसार ही कर्म करूँगा।
संपूर्ण योग का प्रकाशन कर दिया गया है, शिक्षा का परम वचन दे दिया गया है, और चुनी हुई मानव आत्मा अर्जुन एक बार पुनः, अपने अहंमय मन के साथ नहीं, वरन् इस महत्तम आत्म-ज्ञान के साथ, कर्म की ओर मुड़ गया है। भगवान् की विभूति अर्जुन मानवजीवन के अंदर दिव्य जीवन के लिए तैयार हो गया है, उसकी सचेतन आत्मा मुक्त जीव के कर्मों, 'मुक्तस्य कर्म' के लिए प्रस्तुत हो गयी है। मन का मोह नष्ट हो चुका है; अपने स्वरूप और अपने सत्य के विषय में, जो कि हमारे जीवन के भ्रांतिजनक दृश्यों एवं रूपों के कारण इतने काल तक छुपा हुआ था, जीव को स्मृति पुनः प्राप्त हो गयी है तथा उसकी सामान्य चेतना का अंग बन गयी हैः समस्त भ्रम-संशय दूर हो गया है, वह आदेश के पालन में प्रवृत्त हो सकता है और हमारी सत्ता के स्वामी, काल और विश्व में अभिव्यक्त विश्व-पुरुष एवं परमेश्वर उसे अपने लिए तथा जगत् के लिए जिस भी कर्म में नियुक्त करें, जो भी काम सौंपें उसे निष्ठापूर्वक संपन्न कर सकता है।
सञ्जय उवाच
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ।। ७४।।
७४. सञ्जय ने कहाः इस प्रकार मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रोमांचकारी संवाद को सुना।
व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद् गुह्ममहं योगं परम् ।
योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ।। ७५।।
७५. मैंने व्यासजी की कृपा से स्वयं साक्षात् योगेश्वर श्रीकृष्ण के द्वारा वर्णित इस परम गुह्य योग को सुना है।
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ।। ७६।।
७६. हे राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत और पवित्र संवाद को ज्यों-ज्यों मैं बार-बार स्मरण करता हूँ त्यों-ही-त्यों मैं बारंबार हर्ष से रोमांचित हो जाता हूँ।
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यन्द्भुतं हरेः ।
विस्मयो मे महान् राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ।। ७७।।
७७. और हे राजन् ! भगवान् श्रीहरि (कृष्ण) के उस अत्यंत अद्भुत रूप को जितना ही मैं स्मरण करता हूँ उतना ही अधिक मुझे आश्चर्य हो रहा है और मैं बार-बार हर्ष से पुलकायमान होता हूँ।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।। ७८।।
७८. जहाँ कहीं भी योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ कहीं भी धनुर्धारी पार्थ हैं वहाँ निश्चय ही श्री, विजय और समृद्धि और सत्य का अचल धर्म है - ऐसा मेरा विश्वास है।
गीता के संदेश को, इसके दिव्य गुरु के उपदेश को सार-रूप में इस प्रकार कह सकते हैं, "कर्म का रहस्य समस्त जीवन एवं अस्तित्व के रहस्य के साथ एक है। जगत्-अस्तित्व प्रकृति का एक यंत्र मात्र नहीं है, नियम का एक ऐसा पहिया नहीं है जिसमें जीव एक क्षण के लिए या युगों के लिए फँसा हुआ है; यह तो परमात्मा की एक सतत् अभिव्यक्ति है। जीवन केवल जीवन के लिए नहीं वरन् परमेश्वर के लिए है, और मनुष्य का जीवात्मा भगवान् का सनातन अंश है। कर्म आत्म-खोज, आत्म-परिपूर्णता एवं आत्म-साक्षात्कार के लिए है न कि केवल उसके अपने तत्काल या भविष्य में प्राप्त होने वाले बाह्य एवं प्रत्यक्ष फलों के लिए। सभी वस्तुओं का एक आंतरिक विधान एवं अर्थ है जो अध्यात्मसत्ता की परम प्रकृति तथा व्यक्त प्रकृति पर अवलंबित के अर्थ का वास्तविक सत्य उसी के अन्दर निहित है और मन तथा उसके कर्म के बाह्य आकारों में तो उस सत्य को केवल यदा-कदा ही, अपूर्ण रूप से तथा अज्ञान द्वारा प्रच्छन्न रूप में ही प्रकट किया जा सकता है। अतः, कर्म का अमोच्च, निर्दोष एवं व्यापकतम विधान है किसी बाह्य आदर्श एवं धर्म का अनुसरण न करके अपनी उच्चतम तथा अंतरतम सत्ता का सत्य ढूँढ़ निकालना और उसमें निवास करना। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक समस्त जीवन एवं कर्म एक अपूर्णता, एक कठिनाई, एक संघर्ष एवं एक समस्या ही बना रहेगा। केवल अपनी सच्ची आत्मा को ढूँढ़ने तथा उसके सच्चे सत्य एवं वास्तविक स्वरूप के अनुसार जीवन बिताने से ही उस समस्या को अंतिम रूप से हल किया जा सकता है, उस कठिनाई एवं संघर्ष को पार किया जा सकता है और उपलब्ध की जा चुकी आत्मा एवं अध्यात्मसत्ता की सुरक्षित स्थिति में तुम्हारे कर्म पूर्णता को प्राप्त होकर वास्तविक दिव्य कर्म में परिणत हो सकते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को जानो; अपनी वास्तविक आत्मा को ईश्वर समझो और उसे अन्य सबकी आत्मा के साथ एक जानो; अपनी अंतरात्मा को परमेश्वर का एक अंश जानो। और फिर जो जानते हो उसी ज्ञान में निवास करो; अपनी आत्मा में स्थित रहो, अपनी परा आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करो, भगवान् के साथ योगयुक्त होओ और भगवत्तुल्य बनो। सर्वप्रथम, अपने सभी कर्म यज्ञ-रूप में उनके प्रति अर्पित करो जो तुम्हारे अन्दर परमोच्च और एकमेव सत्ता के रूप में विराजमान हैं और जगत् में भी परमोच्च और एकमेव सत्ता के रूप में विराजमान हैं; अन्त में, जो कुछ तुम हो और जो कुछ तुम करते हो वह सब उन्हीं के हाथों में सौंप दो जिससे कि वे परम और विश्वगत भगवान् इस जगत् में तुम्हारे द्वारा अपने संकल्प और अपने कर्मों को संपन्न करें। यही है वह समाधान जो मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ और अन्त में तुम पाओगे कि इसके अतिरिक्त और कोई समाधान है ही नहीं।"
यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है कि "कर्म का परमोच्च, निर्दोष एवं व्यापकतम विधान है किसी बाह्य आदर्श एवं धर्म का अनुसरण न करके अपनी उच्चतम तथा अंतरतम सत्ता का सत्य ढूँढ़ निकालना और उसमें निवास करना।" किसी भी बाह्य विधान की अपेक्षा व्यक्ति को अपनी अंतरतम सत्ता से जो प्रेरणा आती है उसे ही सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहिये। ऐसा करने में मनुष्य की तर्क बुद्धि काँप उठती है क्योंकि तब कर्म तर्कबुद्धि की पकड़ में आने वाले विधानों को अवहेलना कर भीतरी प्रेरणा के आधार पर चलता है। हमारी तर्क बुद्धि किसी ऐसे कर्म को तो स्वीकृत कर सकती है जो कि किन्हीं तय विधानों के अनुसार चले या जो उसके लिए ग्राह्य हो, परंतु जब बुद्धि से परे किसी उच्चतर तथा गहनतर विधान की क्रिया लागू होती है तब तर्कबुद्धि के सारे मापदंडों की उपेक्षा हो जाती है। ऐसे में कोई भी आधार न मिलने के कारण तर्कबुद्धि काँप उठती है।
अतः जीवन का सार यही है कि अपने सभी कर्मों को, अपने भावों को, अपनी संपूर्ण सत्ता को पूरी तरह भगवान् के हाथों में सौंप दिया जाए और तब वे हमारे साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें। हालाँकि यह उक्ति कि 'सब कुछ भगवान् के हाथों में सौंप दो' सुनने में तो सहज प्रतीत होती है परंतु इसके वास्तविक क्रियान्वयन में बड़े भारी धोखे हैं। व्यक्ति को पग-पग पर अनेकानेक प्रलोभनों, संदेहों, संशयों आदि के द्वारा गुजरना होता है। व्यक्ति को बीच के किसी भी पड़ाव पर यह भ्रम हो सकता है कि वह अपने गंतव्य तक पहुँच गया है। यह एक बड़ी ही आम बात है। साधना के मार्ग में किसी क्षुद्र से अनुभव में ही व्यक्ति का अहं फूल सकता है और उसी पड़ाव को वह अंतिम मानकर वहाँ ठहर सकता है। साधना के मार्ग में ऐसे धोखों से बचना लगभग असंभव है। यह व्यक्ति की सच्चाई और निष्कपटता पर निर्भर है कि वह किस हद तक धोखों से बच सकता है। व्यक्ति में जितनी ही अधिक सच्चाई होगी धोखों की आशंका उतने अनुपात में कम होगी। परंतु फिर भी सच्चा मनोभाव तो यह है कि भले कितने भी जाल-घात क्यों न हों, कितने भी विचलन या कितनी भी लड़खड़ाहटें क्यों न हों, व्यक्ति एकनिष्ठ रूप से अपने मार्ग पर चलता ही रहेगा। इसी संदर्भ में श्रीमाताजी कहती हैं, "... यह मत भूलो कि तुम यदि सच्चे प्रयत्न भी करते हो तो भी तुम इन सब कठिनाइयों के अंत तक एक दिन में, एक महीने में, एक वर्ष में नहीं पहुँच जाओगे। जब तुम आरंभ करते हो तब तुम्हें एक अटूट धैर्य के साथ आरंभ करना चाहिये। तुम्हें यह कहना होगा, 'भले इसमें पचास वर्ष लगें, भले इसमें सौ वर्ष लगें, यहाँ तक कि चाहे इसमें अनेक जीवन भी क्यों न लगें, तो भी मैं जो कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ उसे मैं अवश्य प्राप्त करूंगा।'
एक बार यदि तुमने ऐसा करने का निश्चय कर लिया, एक बार यदि तुम बिल्कुल सचेतन हो चुके हो कि चीजें ऐसी ही हैं और यह लक्ष्य सतत् और स्थायी रूप से प्रयत्न करने का कष्ट उठाए जाने योग्य है, तो तुम आरंभ कर सकते हो। अन्यथा, कुछ समय बाद तुम क्लांत हो जाओगे; तुम निरुत्साहित हो जाओगे, तुम अपने-आप से कहोगे, "ओह! यह तो बड़ा कठिन है - मैं इसे करता हूँ और यह चौपट हो जाता है, मैं - फिर करता हूँ और यह फिर चौपट हो जाता है, और फिर मैं इसे दुबारा करता हूँ और यह हमेशा ही चौपट हो जाता है...। फिर क्या किया जाए? कब मैं वहाँ पहुँचूँगा?" अतएव व्यक्ति में प्रचुर धैर्य होना चाहिये। यह कार्य सौ बार चौपट हो सकता है, और तुम इसे फिर से एक सौ एकवीं बार करोगे; यह हजार बार चौपट हो सकता है और तुम फिर से इसे एक हजार एकवीं बार करोगे जब तक कि अंततः यह चौपट नहीं होगा। और अंत में यह चौपट नहीं होता।" (CWM 4, 334-35)
इस प्रकार अठारहवाँ अध्याय 'मोक्षसंन्यासयोग' समाप्त होता है।
परिशिष्ट
I. श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता और उनकी आध्यात्मिक यथार्थता
अंतरस्थ भगवान् मनुष्य में सनातन अवतार हैं; मानव अभिव्यक्ति तो बाह्य जगत् में उसका चिह्न और उसका विकास है.... यह सही है कि भौतिक रूप में ईश्वर के अवतार का गीता में बहुत अधिक विस्तार नहीं है, परंतु निश्चय ही गीता की शिक्षा की श्रृंखला में इसका एक सुनिश्चित स्थान है और ऐसा गीता की संपूर्ण योजना में अंतर्निहित है, जिसकी कि संपूर्ण रूपरेखा ही यह है कि अवतार एक विभूति को, उस मनुष्य को जो महज मानवता की उच्चतम अवस्था तक पहुँच चुका है, दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों की ओर ले जा रहे हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मानव जीव को अपने-आप में उठाने के लिये भगवान् का आंतरिक अवतरण मुख्य बात है - आन्तरिक कृष्ण, बुद्ध या ईसा का ही वास्तविक महत्त्व है। परंतु जिस प्रकार आन्तरिक विकास के लिए बाह्य जीवन का अत्यंत महत्त्व है, ठीक उसी प्रकार इस महान् आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए बाह्य अवतार का भी कोई कम महत्त्व' नहीं है। मानसिक और शारीरिक प्रतीक की परिपूर्णता आंतरिक सद्वस्तु के विकास में सहायक होती है; बाद में यही आंतरिक सद्वस्तु और भी अधिक शक्ति के साथ बाहरी जीवन के द्वारा अपने-आप के और अधिक पूर्ण प्रतीक के रूप में अपने-आप को प्रकट करती है। आध्यात्मिक सद्वस्तु और मानसिक तथा भौतिक अभिव्यक्ति इन दोनों के बीच, सतत् रूप से एक दूसरे पर परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया के द्वारा मानवजाति में भागवत् अभिव्यक्ति ने सदा छिपाव एवं प्रकटन के चक्रों में गति करना स्वीकार किया है ।
प्रश्न : जब श्रीअरविन्द कहते हैं कि 'अंतरस्थ भगवान् मनुष्य में सनातन अवतार हैं', तो इस दृष्टिकोण से तो सभी अवतार ही हुए?
उत्तर : सनातन अवतार का पहलू तो ठीक है, परंतु यहाँ उसकी बाह्य अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। गीता तो इस बारे में बिल्कुल असंदिग्ध रूप से अवतार के रूप में जन्म ग्रहण और जीव के रूप में जन्म ग्रहण में भेद करती है। अवतार के रूप में जन्म ग्रहण करने में वे अपनी पराप्रकृति को अपने वशीभूत करके, उस पर अधिष्ठित होकर जन्म ग्रहण करते हैं जबकि जीव के रूप में जन्म ग्रहण करने में वे अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करते हैं। अंतरस्थ भगवान् का मनुष्य में जो सनातन अंश है वह वास्तव में अवतार के आने से फलीभूत होता है। जब अवतार आते हैं तब जिनका भी उनसे संपर्क साधित होता है उनकी आत्मा के लिए वह अवतार स्वयं इस प्रकार संकल्प कर सकता है मानो वह संकल्प स्वयं उस आत्मा ने ही किया हो। इससे व्यक्तिगत साधना का सारा भार ही समाप्त हो जाता है। श्रीअरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी में भी सभी यह जानते थे कि व्यक्ति को केवल अपने आप को श्रीमाताजी के प्रति खुला रखना है, शेष सभी कुछ तो श्रीमाँ स्वयं ही करती हैं। जीव की प्रगति का इससे त्वरित, प्रभावशाली और शक्तिशाली तरीका नहीं हो सकता। यही अवतार का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस पुस्तक के प्रथम भाग के परिशिष्ट में श्रीमाताजी ने भागवत् अवतारों का यही रहस्य बताया है।
_____________________
*अवश्य ही पार्थिव चेतना के लिए यह तथ्य मात्र भी कि भगवान् अपने-आप को अभिव्यक्त करते हैं, सभी वैभवों में महानतम वैभव है। यहाँ व्याप्त अंधकार को देखो और सोचो कि इसका क्या हाल होता यदि भगवान् इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करते और अंधकार में से ज्योतियों की ज्योति प्रस्फुटित नहीं होती - क्योंकि यही तो अभिव्यक्ति का अर्थ है।
***
इतिहास में चार महान् घटनाएँ हैं, ट्रॉय की घेराबंदी, ईसा का जीवन-चरित व उन्हें सूली पर चढ़ाए जाना, वृंदावन में कृष्ण का निर्वासन तथा कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन-कृष्ण संवाद। ट्रॉय की घेराबंदी ने हेलस (Hellas) को जन्म दिया, वृन्दावन में प्रवास ने भक्तिमय धर्म को जन्म दिया क्योंकि उससे पहले केवल ध्यान-चिंतन व आराधना ही थे, अपने सूलीकरण से ईसा ने यूरोप को मानवीय बनाया और कुरुक्षेत्र का संवाद अभी भी मानवजाति को मुक्त करेगा। और फिर भी कहा जाता है कि इन चारों में से कोई भी घटना कभी घटित ही नहीं हुई।
लोग कहते हैं कि ईसा की शिक्षाएँ फर्जी हैं और कृष्ण कवियों का एक सृजन हैं। (यदि ऐसा है) तो इन फर्जियों के लिए भगवान् का लाख-लाख शुक्रिया अदा करो और इन रचयिता कवियों के आगे प्रणाम करो।
***
निःसंदेह ऐतिहासिक श्रीकृष्ण भी थे। पहले-पहल यह नाम हम छांदोग्य उपनिषद् में पाते हैं जहाँ इनके बारे में हम जो कुछ पता कर पाते हैं वह इतना ही है कि आध्यात्मिक परंपरा में वे एक ब्रह्मवेत्ता के रूप में सुप्रसिद्ध थे, अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन चरित में निःसंदेह इतने सुप्रसिद्ध थे कि केवल देवकी-पुत्र कृष्ण कहकर उन्हें संबोधित करना भर पर्याप्त था कि लोग जान जाते थे कि किसकी चर्चा हो रही है। इसी उपनिषद् में हम विचित्रवीर्य के पुत्र राजा धृतराष्ट्र के नाम का उल्लेख भी पाते हैं, और, चूँकि परंपरा ने इन दोनों नामों को इतने घनिष्ठ रूप से एक-दूसरे से संबद्ध किया है कि ये दोनों ही महाभारत के प्रमुख व्यक्ति हैं, इसलिए हम यह भली-भाँति निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये दोनों वास्तव में समकालीन थे और यह कि इस महाकाव्य में अधिकतर ऐतिहासिक पात्रों की ही चर्चा हो रही है और कुरुक्षेत्र के युद्ध के संबंध में एक ऐसी ही ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है जिसकी छाप इस जाति के स्मृति-पट पर दृढ़ रूप से अंकित थी। हम यह भी जानते हैं कि ईसा-पूर्व की शताब्दियों में श्रीकृष्ण और अर्जुन धार्मिक पूजा के पात्र थे; और, यह मान लेने का कुछ कारण तो है कि यह पूजा किसी ऐसी धार्मिक या दार्शनिक परंपरा के संबंध के कारण ही होती होगी, जहाँ से गीता ने अपने बहुत-से तत्त्वों को, यहाँ तक कि ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय के आधार को भी लिया होगा, और कदाचित् यह भी माना जा सकता है कि ये मानव कृष्ण ही इस संप्रदाय के प्रवर्तक, पुनः-संस्थापक या कम-से-कम प्रारंभिक आचार्यों में से एक रहे होंगे। इसलिए भले ही गीता का बाद का रूप जैसा भी बदल गया हो, तो भी यह भारतीय चिंतन में श्रीकृष्ण के ही उपदेश के परिणाम को प्रस्तुत करता है और संभवतः इस उपदेश का ऐतिहासिक श्रीकृष्ण के साथ तथा अर्जुन और कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ संबंध केवल नाटकीय कल्पना से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। महाभारत में श्रीकृष्ण को एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व और अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है; इसका अर्थ है कि उनकी उपासना और उनके अवतार-तत्त्व की मान्यता उस समय तक – स्पष्ट रूप से पाँचवीं से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक - अवश्य ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी जब भरतवंशियों की प्राचीन कथा और कविता या महाकाव्य-परंपरा ने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया। इस काव्य में अवतार की बाल-वृंदावन-लीला की कथा या किंवदंती का भी संकेत है जिसे पुराणों ने इतने तीव्र और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में वर्णित किया है और जिसने भारत के धार्मिक मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। हरिवंश में भी श्रीकृष्ण के जीवनचरित का वर्णन है, जो बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसे उपाख्यानों से भरा है जो कदाचित् पुराणों में आए वर्णनों का आधार बने हैं।
***
जाति की प्रतिभा तथा एक राष्ट्र की चेतना के विषय में यह सब स्पष्टीकरण, कि वह देवताओं और उनके रूपों की सृष्टि करती है, एक बहुत ही अपूर्ण, बहुत-कुछ छिछला और अपने-आप में एक भ्रमोत्पादक सत्य है। मनुष्य का मन एक मूल स्रष्टा नहीं है, वह तो एक मध्यस्थ है; सृजन करना आरंभ करने के लिये उसे विश्व-चेतना से एक प्रवर्तनकारी 'अंतःप्रेरणा', कोई संदेश या कोई संकेत अवश्य प्राप्त होना चाहिये और उसे लेकर वह जो कुछ कर सकता है वह करता है। ईश्वर हैं, परंतु ईश्वर के संबंध में मनुष्य की अवधारणाएँ उसकी अपनी मानसिकता में कभी तो भगवान् की, कभी अन्य सत्ताओं और शक्तियों की प्रतिबिम्ब होती हैं और मनुष्य के पास जो सूचनाएँ आती हैं वे तब तक साधारणतया बहुत अपूर्ण और आंशिक होती हैं जब तक कि वे अभी भी मानसिक होती हैं, जब तक कि मनुष्य एक उच्चतर और सत्यतर, एक आध्यात्मिक या गुह्य ज्ञान तक नहीं पहुँच गया होता। देवताओं का अस्तित्व पहले से ही है, वे मनुष्य के द्वारा रचे नहीं गए हैं, भले ही वह उनकी अवधारणा स्वयं अपनी ही प्रतिमूर्ति में करता प्रतीत होता है; - मूलभूत रूप से, विश्वगत 'सद्वस्तु' से वह देवताओं के विषय में जो सत्य ग्रहण करता है उसे ही यथाशक्ति आकार प्रदान करता है। किसी कलाकार या किसी भक्त को देवताओं का एक दर्शन प्राप्त हो सकता है और वह दर्शन उस जाति की चेतना में स्थिर और सर्वसामान्य बन सकता है और उस अर्थ में यह सत्य हो सकता है कि मनुष्य देवताओं को उनके आकार प्रदान करता है; परंतु वह इन आकारों का आविष्कार नहीं करता, वह तो जो कुछ देखता है बस उसे ही अंकित करता है; जो आकार वह उन्हें देता है वे स्वयं उसे प्राप्त होते हैं। श्रीकृष्ण के "परंपरागत" रूप में मनुष्यों ने वह सब मूर्तिमान् किया है जो कुछ अंश वे उनके शाश्वत सौंदर्य का देख पाये और जो कुछ उन्होंने देखा है वह सत्य भी हो सकता है और सुन्दर भी, वह उस रूप का कुछ अंश प्रकट करता है, परंतु यह काफी कुछ निश्चित ही है कि यदि उस शाश्वत सौंदर्य का कोई शाश्वत रूप है तो उस रूप का जो कुछ भी अंश देखने में अब तक मनुष्य समर्थ हुआ है उससे वह हजार गुना अधिक सुन्दर है। भारत माता भूमि का कोई खण्ड नहीं है; वह एक शक्ति है, एक देवी है क्योंकि सभी राष्ट्रों की ऐसी एक देवी होती हैं जो उनके पृथक् अस्तित्व को थामे रखती है व उन्हें अस्तित्वमान बनाए रखती है। ऐसी सत्ताएँ उन लोगों, जिन्हें ये प्रभावित करती हैं, जितनी ही यथार्थ या उनसे भी अधिक स्थायी रूप से यथार्थ होती हैं। परंतु वे एक उच्चतर लोक की होती हैं, वैश्विक चेतना व सत्ता का अंग होती हैं और यहाँ पृथ्वी पर मानव चेतना को, जिस पर कि ये अपना प्रभाव डालती हैं, गढ़कर अपना कार्य करती हैं। मनुष्य के लिए, जो केवल अपनी ही वैयक्तिक, राष्ट्रीय या जातीय चेतना को कार्यरत देखता है और यह नहीं देखता कि कौन-सी चीज उसकी चेतना पर कार्य करती और उसका गठन करती है, यह सोचना स्वाभाविक ही है कि सभी कुछ उसके स्वयं के द्वारा सृजित होता है और उसके पीछे कोई भी विश्वमय तथा महत्तर चीज नहीं है। श्रीकृष्ण-चेतना एक यथार्थता है, परंतु यदि कोई कृष्ण ही न हो तो फिर कोई कृष्ण चेतना भी नहीं हो सकती; किसी मनमानी तात्त्विक सूक्ष्मकल्पना के अतिरिक्त, किसी सचेतन पुरुष के बिना कोई चेतना हो ही नहीं सकती। व्यक्ति ही है जो व्यक्तित्व को मूल्य और यथार्थता प्रदान करता है, वह उसके अंदर स्वयं को अभिव्यक्त करता है पर उसके द्वारा गठित नहीं होता। श्रीकृष्ण एक सत्ता हैं, एक पुरुष हैं और दिव्य पुरुष के रूप में ही हम उनसे मिलते, उनकी वाणी सुनते, उनसे बातें करते और उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। कृष्ण की चेतना के विषय में ऐसे चर्चा करना कि वह कृष्ण से पृथक् कोई चीज है, उस मन की एक भूल है जो सदा ही अविभेद्य को विभक्त करता रहता है और जिसमें निराकार को ही, क्योंकि वह अमूर्त है, साकार से अधिक महान्, अधिक सत्य और अधिक स्थायी मानने की प्रवृत्ति रहती है। ऐसे विभेद मन के अपने प्रयोजनों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, परंतु यह यथार्थ सत्य नहीं है; यथार्थ सत्य में सत्ता या व्यक्ति तथा उसकी निर्व्यक्तिकता अथवा सत्ता की अवस्था एक ही यथार्थता हैं।
प्रश्न : इस पंक्ति का क्या अर्थ है: "देवताओं का अस्तित्व पहले से ही है, वे मनुष्य के द्वारा रचे नहीं गए हैं, भले ही वह उनकी अवधारणा स्वयं अपनी ही प्रतिमूर्ति \mathfrak{F} करता प्रतीत होता है; - मूलभूत रूप से, विश्वगत 'सद्वस्तु' से वह देवताओं के विषय में जो सत्य ग्रहण करता है उसे ही यथाशक्ति आकार प्रदान करता है।"
उत्तर : मनुष्य जब देवताओं की कल्पना करता है तब वे उसके लिए बहुत कुछ मानवीय आकार में प्रकट होते हैं। वे मानव रूप से कुछ-कुछ भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि गणेश का मुख मानव आकार से भिन्न है, कुछ देवताओं के दो हाथों की बजाय अनेक हाथ होते हैं, आदि-आदि। परंतु फिर भी मोटे तौर पर सभी देवताओं का रूप मनुष्य के समान ही होता है। अतः मनुष्य को प्रतीत होता है कि देवताओं को वह अपनी मानसिक धारणा के आधार पर आकार प्रदान करता है। परंतु वास्तव में तो देवताओं की प्रेरणा से ही मनुष्य वैसी कल्पना कर पाते हैं क्योंकि देवताओं का स्वरूप हमें जो प्रतीत होता है केवल उसी से सीमित नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण का स्वरूप किन्हीं भी पुराणों आदि में आज तक भी जैसा वर्णित हुआ है उसी से बिल्कुल भी सीमित नहीं हो सकता। अतः मनुष्य जो कुछ भी कल्पना करते हैं और आगे भी कर सकते हैं, उस सब को मिलाकर भी किसी देवता का पूरा स्वरूप उजागर नहीं हो सकता। साथ ही, जो रूप हमें दिखाई देता है वह हमें अपने सामूहिक अवचेतन के कारण भी वैसा दिखाई देता है। कोई हिन्दुस्तानी किसी देवता को जिस रूप में देखेगा उसी देवता को कोई यूनानी किसी अन्य रूप में देखेगा। अतः जाति भेद के कारण भी यह भेद उत्पन्न हो जाता है। हमारा मन तो केवल उस रूप के विषय में संकेतों को ग्रहण करता है, वह उन रूपों का स्रष्टा नहीं होता। इस अर्थ में, स्वयं देवता ही उसे जो रूप दिखाना चाहते हैं वैसा उसके समक्ष या उसकी कल्पना में प्रकट करते हैं। देवता ही नहीं, अपितु किसी राष्ट्र की आत्मा भी किसी मानव व्यक्तित्व में अपने आप को प्रकट करके अपनी बात को उद्घोषित कर सकती है जैसा कि भारत की आत्मा ने स्वामी विवेकानंद के और श्रीअरविन्द के द्वारा तथा अतीत में अन्य कुछ लोगों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। यही नहीं, हमारी सभी छोटी-बड़ी घटनाओं के पीछे, इच्छा, कामना, लालसा, क्रोध, रोग आदि के पीछे सूक्ष्म सत्ताएँ होती हैं जो अपने आप को हमारे द्वारा अभिव्यक्त करती हैं। चूंकि हमारी दृष्टि बहुत ही संकीर्ण है इसलिए हमें सूक्ष्म जगतों का आभास कदाचित् ही होता है इसीलिए हम इन सब चीजों को देख और समझ नहीं पाते। परंतु मनुष्य में यह संभावना है कि वह इतना विकसित हो जाए कि उन सत्ताओं की कठपुतली न रहकर उनका स्वामी बन जाए।
कृष्ण की ऐतिहासिकता आध्यात्मिक दृष्टि से गौण महत्त्व की है और कोई अनिवार्य चीज नहीं है, परंतु फिर भी इसकी भारी महत्ता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई युक्तियुक्त संदेह उठ सकता है कि मनुष्य रूपी कृष्ण कोई पौराणिक या कोई काव्यात्मक आविष्कार नहीं हैं अपितु वे वास्तव में पृथ्वी पर विद्यमान थे और भारत के अतीत में अपनी एक भूमिका निभाई धौ। दो तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं, एक यह कि वे एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक व्यक्तित्व माने जाते थे, ऐसे व्यक्तित्व जिनका आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना एक उपनिषद् में अभिलिखित है, और दूसरे यह कि वे परंपरागत रूप से एक दिव्य मनुष्य माने जाते थे, जो अपनी मृत्यु के पश्चात् एक देवता के रूप में पूजे गये हैं; यह महाभारत और पुराणों की कहानी के अलावा है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भागवत् धर्म, जो कि भारतीय आध्यात्मिकता के प्रवाह में एक महत्त्वपूर्ण धारा है, के साथ उनके नाम का संबंध महज किसी पौराणिक कथा या कवि-कल्पना के आविष्कार के ऊपर आधारित था। महाभारत एक काव्य है, इतिहास नहीं है परंतु स्पष्ट रूप से यह एक ऐसा काव्य है जो एक महान् ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जिसे कि परंपरा से स्मृति में सुरक्षित रखा गया है; इससे संबंधित कुछ व्यक्ति, जैसे धृतराष्ट्र, परीक्षित आदि निश्चय ही विद्यमान थे और एक नेता, योद्धा और राजनीतिज्ञ के रूप में कृष्ण ने जो भूमिका निभाई थी उसकी कथा का अपने-आप में संभाव्य तथा बाह्य रूप में एक ऐसी परंपरा पर आधारित होना स्वीकार कर सकते हैं जिसे ऐतिहासिक मूल्य दिया जा सकता है और जो एक पौराणिक या महज काव्यात्मक आविष्कार का ही हाव-भाव नहीं रखती। बस, सैद्धांतिक युक्तितर्क की दृष्टि से मानवरूपी कृष्ण के ऐतिहासिक व्यक्ति होने के विषय में निश्चित रूप से इतना ही कहा जा सकता है; परंतु मेरी दृष्टि में इसमें इससे और बहुत अधिक बात है और मैंने सदा ही भगवान् के अवतार को एक सत्य घटना के रूप में स्वीकार किया है; और कृष्ण की ऐतिहासिकता को उसी तरह स्वीकार किया है जैसे कि ईसा की ऐतिहासिकता को माना है।
श्रीकृष्ण ऐतिहासिक रूप से रहे हैं या नहीं उससे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि वे आज भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। वे ऐतिहासिक रहे भी हों तो भी उससे हमें क्या प्रयोजन हो सकता है यदि आज हमें उनकी जीवंत उपस्थिति महसूस न होती हो। आज यदि हम उनकी उपस्थिति को अनुभव न कर पाते तब तो उनका प्रभाव वैसा ही निष्प्रभावी होता जैसा किसी भी अन्य ऐतिहासिक व्यक्तित्व का होता है। इसी तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि भगवान् शंकर ने कोई भौतिक शरीर न धारण किया हो, परंतु उनका पार्थिव चेतना में जितना सक्रिय प्रभाव है उसे तो नकारा ही नहीं जा सकता। और यह उपस्थिति ही है जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण चीज है।
वृंदावन की कहानी एक दूसरा ही मामला है; यह महाभारत की मुख्य कहानी में नहीं आती और इसका उद्गम पौराणिक है और यह बात कही जा सकती है कि इस कहानी के एक प्रतीकात्मक स्वरूप के होने की बात को आरंभ से ही माना जाता रहा है। एक समय मैंने भी उस व्याख्या को स्वीकार किया था, पर बाद में मुझे इसे छोड़ना पड़ा; पुराणों में ऐसी कोई चीज नहीं जो ऐसे किसी आशय की झलक देती हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहानी किसी ऐसी चीज से संबंधित है जो वास्तव में कहीं घटी थी या घटित होती है। गोपियाँ पुराणों के लिये वास्तविक व्यक्ति हैं न कि प्रतीक। यह उनके लिये कम-से-कम एक गुह्य सत्य था, तथा गुह्य और प्रतीकात्मक एक ही चीज नहीं हैं; प्रतीक एक अर्थपूर्ण मानसिक रचनामात्र अथवा एक काल्पनिक आविष्कारमात्र हो सकता है, परंतु गुह्य एक ऐसी यथार्थ वस्तु है जो कहीं पर, मानो भौतिक दृश्य के पीछे, वास्तविक है, और जिसका पार्थिव जीवन के लिये अपना सत्य हो सकता है तथा पार्थिव जीवन पर जो उसका प्रभाव पड़ता है वह यहाँ अपने-आप को मूर्तिमान् भी कर सकता है। गोपियों की लीला को इस प्रकार कल्पित किया गया लगता है मानो वह दिव्य गोकुल में निरंतर चल रही है और जिसने अपने-आप को पार्थिव वृंदावन में प्रक्षिप्त कर अभिव्यक्त किया और इसे सदा ही अनुभूत किया जा सकता है तथा इसके अर्थ को अंतरात्मा के अंदर क्रियान्वित अथवा यथार्थ बनाया जा सकता है। यह बात मानी जा सकती है कि पुराणों के लेखकों ने ऐसा मान लिया था कि वह लीला वास्तव में अवतार कृष्ण के जीवन में पृथ्वी पर प्रक्षिप्त हुई थी और भारत के धार्मिक मन द्वारा भी इसे इसी रूप में स्वीकार किया गया है।
इन प्रश्नों का और जिन अटकलों को इन्होंने जन्म दिया है उनका आध्यात्मिक जीवन के साथ कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। वहाँ जो चीज मायने रखती है वह है कृष्ण के साथ संपर्क और कृष्ण-चेतना की ओर विकास, आत्मा में उनकी उपस्थिति, उनसे आध्यात्मिक संबंध और उनके साथ मिलन; और जब तक वह प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसकी अभीप्सा बनाये रखना, भक्ति में अग्रसर होते रहना तथा पथ पर जितना भी ज्ञान प्राप्त किया जा सके उसे प्राप्त करना। जिसे ये सब चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, जो कृष्ण के सान्निध्य में रह चुका है, उनकी वाणी सुन चुका है, उनको सखा या प्रेमी, मार्गदर्शक, गुरु, प्रभु के रूप में जान चुका है अथवा, उससे भी अधिक, अपनी समूची चेतना उनके संपर्क से परिवर्तित कर चुका है, अथवा अपने भीतर उनकी उपस्थिति को अनुभूत कर चुका है, उसके लिए ऐसे प्रश्नों में केवल एक बाहरी और सतही रुचि ही शेष रहती है। इसी तरह, जिसे आंतरिक वृंदावन और गोपियों की लीला के साथ संपर्क प्राप्त हो चुका है, जो आत्मसमर्पण कर चुका है, जो आनंद और सौन्दर्य के सम्मोहन के वशीभूत हो चुका है अथवा केवल वंशी की ध्वनिमात्र की ओर ही मुड़ चुका है, उसके लिये शेष सबका कदाचित् ही कोई मूल्य होता है। परंतु दूसरे दृष्टिकोण से, यदि कोई अवतार की ऐतिहासिक सत्यता को स्वीकार कर सके तो उसे यह महान् आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा कि उसे इस विश्वास के कारण कहीं अधिक ठोस अनुभूति प्राप्त करने का आश्रय-स्थल मिल जायेगा कि कम-से-कम एक बार भगवान् ने प्रत्यक्ष रूप में इस धरा का स्पर्श किया था, पूर्ण अभिव्यक्ति को संभव बनाया था, दिव्य पराप्रकृति के लिए इस क्रमविकसनशील पर अभी भी बहुत अपूर्ण पार्थिव प्रकृति में अवतरित होना संभव बनाया था।
***
तुम मुझसे यह आशा नहीं कर सकते कि मैं श्रीकृष्ण की तुलना में मेरी अपनी आध्यात्मिक महत्ता बताने के लिए बहस करूँ। स्वयं यह प्रश्न ही केवल तभी प्रासंगिक होगा यदि अरविंदवाद और वैष्णववाद जैसे कोई दो परस्पर विरोधी कट्टरपंथी धर्मसंप्रदाय होते जो प्रत्येक अपने ही देव की महत्ता पर आग्रह कर रहे होते। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर किस कृष्ण की सत्ता को मैं चुनौती दूँ या ललकारूँ, गीता के उन कृष्ण को जो परात्पर देवाधिदेव, परमात्मा, परब्रह्म, पुरुषोत्तम, विश्वमय देव, जगत्पति, वासुदेव हैं जो सब कुछ हैं, सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी हैं, या उन परमदेव को जो वृंदावन, द्वारका और कुरुक्षेत्र में अवतरित थे और जो मेरे योग के पथप्रदर्शक थे और जिनके साथ मैंने तादात्म्य प्राप्त किया था? और यह सब मेरे लिए कोई दार्शनिक या मानसिक बात नहीं है अपितु दिन-प्रतिदिन की और हर-एक घंटे की अनुभूति की और मेरी चेतना के द्रव्य के लिए अंतरंग बात है।
***
तब भगवान् ने मेरे हाथों में गीता रख दी। मेरे अंदर उनकी शक्ति प्रवेश कर गई और मैं गीता की साधना करने में समर्थ हुआ। मुझे केवल बौद्धिक रूप से ही नहीं, अपितु अनुभूति द्वारा यह जानना था कि श्री कृष्ण की अर्जुन से क्या माँग थी और वे उन लोगों से क्या माँग करते हैं जो उनका कार्य करने की अभीप्सा रखते हैं, घृणा और कामना-वासना से मुक्त होना, फल की इच्छा न रखकर भगवान् के लिए कर्म करना, अपनी स्वेच्छाचारिता का त्याग करना और भगवान् के हाथों में एक निश्चेष्ट तथा सच्चा यंत्र बनकर रहना, ऊँच और नीच, मित्र और शत्रु, सफलता और विफलता के प्रति समदृष्टि रखना और यह सब होते हुए भी भगवान् के कार्य में लापरवाही न करना।
II. गीता तथा श्रीअरविन्द का संदेश
यह एक तथ्य नहीं है कि गीता श्रीअरविन्द की संपूर्ण शिक्षा का आधार प्रदान करती है; क्योंकि गीता जगत् में जन्म ग्रहण करने से छुटकारे को चरम उद्देश्य या कम-से-कम योग की चरम परिणति के रूप में स्वीकार करती प्रतीत होती है; वह आध्यात्मिक क्रमविकास के विचार को या उच्चतर स्तरों और अतिमानसिक सत्य-चेतना को तथा पार्थिव जीवन के पूर्ण रूपांतर के साधन के रूप में उस चेतना को नीचे उतार लाने के विचार को सामने नहीं लाती।
श्रीअरविन्द के विवेचन के अनुसार अतिमानस, सत्य-चेतना का विचार ऋग्वेद में है और उपनिषदों के एक या दो संदर्भों में है, किंतु उपनिषदों में यह केवल मानसिक, प्राणिक और भौतिक पुरुष को अतिक्रम करने वाले विज्ञानमय पुरुष की अवधारणा में बीजरूप में है; ऋग्वेद में यह विचार है अवश्य परंतु केवल सिद्धांत रूप में, इसका विस्तार या विकास नहीं किया गया है और स्वयं यह सिद्धांत भी हिन्दू परंपरा से लुप्त हो चुका है।
अन्य चीजों के साथ ये बातें भी हैं जो हिंदु परंपरा के साथ तुलना में श्रीअरविंद के संदेश की नवीनता या उसकी पृथक्ता का गठन करती हैं - यह विचार कि संसार न ही कोई माया की सृष्टि है या भगवान् की केवल लीलामात्र है, या अज्ञान के अंदर जन्मों का कोई ऐसा चक्र है जिससे हमें छूट निकलना है, अपितु यह तो अभिव्यक्ति का एक क्षेत्र है जिसमें जड़तत्त्व में आत्मा एवं प्रकृति का एक उत्तरोत्तर क्रमविकास है, जो जड़तत्त्व के द्वारा प्राण और मन से होते हुए मन से परे तब तक होता है जब तक कि यह जीवन में सच्चिदानंद के पूर्ण प्रकाशन तक नहीं पहुँच जाता। यही है जो श्रीअरविंद के योग का आधार है और जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करता है।
***
संदर्भ सूची
इस पुस्तक में गीता के श्लोकों पर प्रस्तुत की गई टीका श्रीअरविन्द व श्रीमाँ की कृतियों से ली गई है। जिन श्लोकों के लिए टीका दी गई है, उनकी श्लोक संख्याओं के सामने उन टीकाओं के संदर्भ दिये गये हैं। प्रस्तावना व परिशिष्ट में उद्धरण जिस पुस्तक से लिये गये हैं उनकी खण्ड संख्या तथा पृष्ठ संख्या दी गई है। (S) का अर्थ है The Synthesis of Yoga (CWSA 23- 24), (L) का अर्थ है Letters on Yoga (CWSA 28 - 31 ) , (Svt.) का अर्थ है Savitri (CWSA 33-34), जहाँ संदर्भों के लिए खण्ड संख्या नहीं दी गई है वे सभी उद्धरण Essays on the Gita (CWSA 19 ) से लिए गए हैं। श्रीअरविन्द की अन्य पुस्तकों के संदर्भों के लिए खण्ड संख्या तथा पृष्ठ संख्या (CWSA vol no : page no.) दी गई है। श्रीमाँ की कृतियों से लिए गए उद्धरणों के लिए खण्ड संख्या तथा पृष्ठ संख्या (CWM Vol no : page no.) दी गई है।
चूंकि यहाँ मुद्रित उद्धरणों का तथा श्लोकों का अनुवाद अनुवादक द्वारा ही किया गया है अथवा अन्य स्थानों पर मूल विचार को अधिक सुगम, स्पष्ट व सटीक बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध अनुवाद में संशोधन व परिवर्तन किए गए हैं इसलिए उद्धरणों के लिए मूल स्रोतों की ही सूची दी गई है।
अध्याय आठ
:291
16:297-98
3:291-92
21:298-99
4:292-94, 292
22:299
6:294,295-96
23:299
10:296
27:299-300
13:297
पादटीका
1:297
2:S556-57
3:299
________________
CWSA: Complete Works of Sri Aurobindo CWM: Collected Works of The Mother
550
अध्याय नौ
1:301,309
3:309-11,316-18
4:311-12
5:318-19
6:319
8:320
10:320-22
II:322-23, 324 - 25
11:325-26
12:326
13:327
14:327
15:327-28
16:328-29
17:329
19:329-30
21:330-31
22:331-32
24:332-33
25:333
26:S163,333
27:333, S111-14
28:333-34
29:334, CWM(7)243
31:334-35
32:335-36
33:336
34:336
पादटीका
1:Svt. 648
2:Svt. 657
3:329
4:CWM(8)234-35
5:L(ii) 70-71
6:CWSA(2)218
अध्याय दस
I:337,343-44
15:356-57,357-58
I:344-45
5:345, 346, 347-51
II:351-54
18:358-59
19:360-61
42:361-62, 361,373-76
II:355-56
पादटीका
1:Svt. 61
2:346-47
3:347
4:Svt.311-12
5:360
अध्याय ग्यारह
I:377
I:377
4:377-78
7:378
30:381-83
31:383-84
32:384-86
34:384
35:388
36:389-90
37:390
40:391
46:391-93
47:393-94
54:394-95
55:395
पादटीका
1:CWSA(12)499
2:S600-02
3:S110
अध्याय बारह
:396-99,398
1:399-400
2:400
4:341,400
5:400-01
7:401-02
8:402
9:402
10:402-03
11:403
12:403-04
19:405
20:405-06
पादटीका
1:CWM(7)247
अध्याय तेरह
:409
I:409-10
3:412
7:412-14
12:414-15
13:S298, 415, CWSA(21)39,
CWSA(21)38
16:416-17
17:CWSA(22)353,
CWSA(21)79
19:S304-06
21:417-18
22:S99-100
23:S431-35
24:CWSA(22)361-62,418
27:Svt. 63
28:Svt. 66-67
29:418-19
30:S215
32:419
35:420
पादटीका
1:412
2:CWSA(21)33
3:CWSA(21)85, CWSA(12)107 4:S305
अध्याय चौदह
:421
2:423-24
4:424
5:425-27, S684-87
9:430-31
10:430
18:190-93
19:S238-39
25:S239,433
27:434
पादटीका
1:422
2:421-22
3:S232
4:S235
5:L(i) 47, S241
अध्याय पंद्रह
:435, 228-30, 442-43
5:444
6:444-45
7:445-46
10:446
11:446
15:447
16:437,439-40
18:440-41,447
20:447-49
पादटीका
1:443-44
2:S275
अध्याय सोलह
:450, 461-65, S689, 467-70
5:470-71
6:471
20:473-74
24:475-76
पादटीका
1:370
2:467
3:468
4:L451-52, L463
5:L465-66
6:472
7:473
अध्याय सत्रह
:477,478,479,480-81
2:483-84
3:482, S628
7:484-85
10:485
11:487-88
12:486-87
13:485-86,489
17:489-90
19:490
20:491
23:491
28:492
अध्याय अठारह
1:493
2:494-95
3:495
7:495-96
8:496
10:496-97
11:497
17:498-99
18:500-01
20:500
22:499-500
23:501
25:501
26:502
27:502
28:502
29:502-03
30:504-05
31:503-04
32:503
37:505,506
38:505-06
39:505
II:508-09
48:510-12, 514-19,520-24
III:526-28
49:529-32
50:532-33
53:533-35
54:535-36
55:536-38
56:538-39
IV:540
62:541-42, 549-50, 542, 550-52,
554-55
64:555-56
66:556-61
73:561
78:572
पादटीका
1:493-94
2:497-98
3:500
4:513
85:S747
6:S748-49
7:534-35
परिशिष्ट
I:15, 167, CWSA(12)427-28, 15-16, L481-484, CWSA(35)431-32, CWSA(8)5-6
II:L(ii), 444-45,
पादटीका
1:L471
श्रीकृष्ण के नाम व उनके अर्थ
अच्युत निष्पाप, अटल, अमोघ 1:21, 11:42, 18:73
अजम् अजन्मा 10:12
अनन्त अनन्त, असीम 11:11, 11:37
अनन्तरूप अनन्त रूप वाले 11:38
अनन्तवीर्य अथाह पराक्रमी, अनन्त तेजयुक्त 11:40
अप्रतिमप्रभाव अतुलनीय तेज या प्रभाव वाले 11:43
अप्रमेय अमित, जिसे नापा न जा सके 11:17
अमित विक्रमः अनन्त पराक्रमी 11:40
अरिसूदन शत्रुओं का संहार करने वाले 2:04
आदिदेवम् मूल या आदि देवता 10:12
ईशम् ईश्वर या प्रभु 11:44
कमलपत्राक्ष कमल के पत्र के समान नेत्र वाले 11:02
कृष्ण जो सभी कुछ को अपनी ओर आकृष्ट 1/28, 1/32, 1/41, 5/1, 6/34, 6/37
करते हैं, समस्त प्राणियों को आकृष्ट 6:39, 11:41, 17:1, 18/75.18 / 78
करने वाले, श्याम वर्ण
केशव सुंदर, लंबे या अत्यलंकृत केश वाले 1:31 2/54, 3/1 10:14, 11:35, 13:1, 18:76
केशिनिसूदन केशि राक्षस का संहार करने वाले 18:01
गोविन्द गोवंश या प्रकाश के संरक्षक 1:32, 2:9
जगत्पते जगत् के ईश्वर 10:15
जगत्रिवास जगतों के निवासस्थान, 11/25, 11/37, 11/45
समस्त जगतों के आश्रय
जनार्दन लोगों को कष्टदेने वाला, दुःखदायी, 1/36, 1/39, 1/44, 3/1, 10/18
कष्टकारी, पीड़ा देना 11:51
दिव्यंपुरुषम् दिव्य पुरुष 10:12
देव ईश्वर, देवता 11:15, 11:44
देवदेव सभी देवों के देव 10:15, 11:13
देववर महान् देव 11:31
देवेश देवताओं के स्वामी 11:25, 11:37, 11:45
धर्मगोप्ता सनातन धर्मों के संरक्षक 11:18
परंधाम परमोच्च स्थिति, परम धाम 10:12, 11:38
परंब्राह्म परम ब्रह्म 10:12
परमेश्वर परम ईश्वर 11:03
परमं अक्षरं परम अक्षर या अपरिवर्तनीय 11:18
परमं पवित्रम् परमोच्च पवित्रता 10:12
पुरुषं शाश्वतम् शाश्वत पुरुष 10:12
पुराणः पुरुषः पुरातन पुरुष 11:38
पुरुषोत्तम परमोच्च पुरुष 8:1, 10:15, 11:3, 15:18, 15:19
प्रभो प्रभु 11:4, 14:21
भगवन् श्रीभगवान् 10:14, 10:17
भूतभावन भूतों अथवा प्राणियों के उद्गम 10:15
भूतेश प्राणियों के ईश्वर 10:15
मधुसूदन मधु राक्षस के संहारक 1:35, 2:1, 2:4, 6:33, 8:2
महात्मन् महान् आत्मा, प्रतापी आत्मा 11:12, 11:20, 11:37, 11:50
महाबाहो शक्तिशाली भुजाओं वाले 6:38, 11:23, 18:1
महायोगेश्वर योग के महान् ईश्वर 11:9
माधव लक्ष्मीपति, मधुर, यदुवंश में मधु के वंशज 1:14, 1:37
यादव यदु वंश के वंशज 11:41
योगिन् योगी 10:17
योगेश्वर योग के ईश्वर 11:4, 18:75, 18:78
वासुदेव वसुदेव के पुत्र, सर्वव्यापी पुरुष 10:37, 11:50, 18:74
वाष्र्णेय वृष्णीवंश के वंशज 1:41, 3:36
विभुं सर्वव्यापी प्रभु 10:12
विश्वमूर्ते विश्वमय रूप 11:46
विश्वरूप विश्वमय रूप 11:16
विश्वेश्वर विश्व के ईश्वर 11:16
विष्णो सर्वव्यापी प्रभु 11:24, 11:30
वेत्ता ज्ञाता 11:38
वेदवित् वेद के ज्ञाता 15:15
वेदान्तकृत् वेदान्त के रचयिता या प्रणेता 15:15
वेद्यम् जो जानने योग्य है 11:38
सनातन पुरुषः सनातन अथवा नित्य पुरुष 11:18
सहस्रबाहो सहस्र भुजाओं वाले 11:46
हरि विष्णु का नाम 11:9, 18:77
हृषीकेश इंद्रियों के स्वामी 1:15, 1:21, 1:24, 2/9.2 / 10
11:36, 18:1
अर्जुन के नाम व उनके अर्थ
अनघ निष्पाप 3:3, 14:6, 15:20
अर्जुन सात्त्विक अथवा पवित्र और 1:4, 1:47, 2:2, 2:45, 3:7, 4:5, 4:9,
प्रकाश से परिपूर्ण आत्मा 4:37, 6:16, 6:32, 6:46, 7:16, 7:26,
8:16, 8:27. 9:19. 10:39, 10:42, 11:47 11:54, 18:9, 18:34, 18:61
कपिध्वज जिसकी ध्वजा पर कपि 1:20
हनुमान का चिह्न है
किरीटी मुकुट से सुशोभित मनुष्य 11:35
कुरुनन्दन कुरु को आनन्द देनेवाले 2:41, 6:43, 14:13
कुरुप्रवीर कुरुओं में अग्रणी 11:48
कुरुश्रेष्ठ कुरुओं में श्रेष्ठ 10:19
कुरुसत्तम कुरुओं में सर्वोत्तम 4:31
कौन्तेय कुन्ती पुत्र 1:27, 2:14, 2:37, 2:60, 3:9, 3:39,
5:22, 6:35, 7:8, 8:6, 9:7, 9:10, 9:23, 9:27, 9:31, 13:2, 13:32, 14:4, 14:7, 16:20, 16:22, 18:48, 18:50, 18:60
गुडाकेश जिसने निद्रा को जीत लिया है 1:24, 2:9, 10:20, 11:7
धनञ्जय धन-संपदा को जीतने वाला 1:15, 2:48, 2:49, 4:41, 7:7, 9:9,
10:37, 11:14, 12:9, 18:29, 18:72
परंतप शत्रुओं का दमन करने वाला 2:3, 4:2, 4:5, 4:33, 7:27, 9:3,
10:40, 11:54,18:41
पाण्डव पाण्डु का पुत्र 1:14, 1:20, 4:35, 6:2, 11:55,
14:22, 16:5
पार्थ पृथा (कुन्ती) का पुत्र 1:26, 2:3, 2:21, 2:32, 2:39, 2:42,
2:55, 2:72, 3:16, 3:22, 3:23, 4:11, 4:33, 6:40, 7:1, 7:10, 8:8, 8:14, 8:22, 8:27, 9:13, 9:32, 10:24, 11:5, 12:7, 16:4, 16:6, 17:26, 17:28, 18:6, 18:30, 18:3, 18:32, 18:33, 18:34, 18:35, 18:72
पुरुषर्षभ मनुष्यों में श्रेष्ठ 2:15
पुरुषव्याघ्र मनुष्यों में व्याघ्र के समान भरतवंशियों में 18:4
सर्वश्रेष्ठ भरतवंशियों में श्रेष्ठ
भरतर्षभ भरतश्रेष्ठ 17:12 3:41, 7:11, 7:16, 8:23,
13:27, 14:12, 18:36
भरतसत्तम भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ 18:4
भारत भरतवंश में उत्पन्न हुआ 2:14, 2:18, 2:28, 2:30, 3:25, 4:7,
4:42, 7:27, 11:6, 13:3, 13:34, 14:3, 14:8, 14:9, 14:10, 15:19, 15:20, 16:3, 17:3, 18:62
महाबाहो शक्तिशाली भुजाओं वाला 2:26, 2:68, 3:28, 3:43, 5:3, 5:6,
6:35, 7:5, 10:1, 14:5, 18:13
सव्यसाचिन् दोनों हाथों से बाण चलाने में निपुण 11:33
![]()
श्रीअरविन्द गीता के संदेश को उस महान् आध्यात्मिक गति का आधार मानते हैं जो मानवजाति को अधिकाधिक उसकी मुक्ति की ओर, अर्थात् मिथ्यात्व और अज्ञान से निकलकर सत्य की ओर ले गई है, और आगे भी ले जाएगी।
अपने प्रथम प्राकट्य के समय से ही गीता का अतिविशाल आध्यात्मिक प्रभाव रहा है; परंतु जो नवीन व्याख्या श्रीअरविन्द ने उसे प्रदान की है, उसके साथ ही उसकी प्रभावशालिता अत्यधिक बढ़ गई है और निर्णायक बन गई है।
- श्रीमाँ