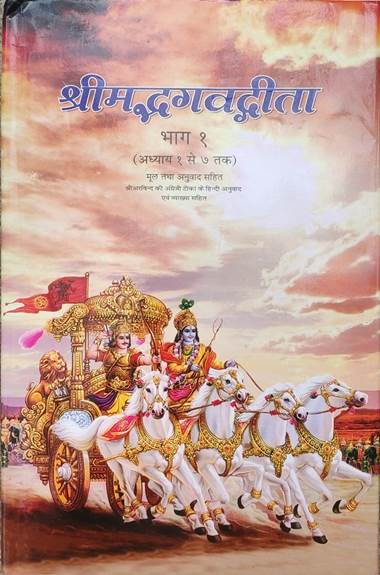
श्रीमद्भगवद्गीता
भाग १
अध्याय १ से ७ तक
श्रीमद्भगवद्गीता भाग १
(अध्याय १ से ७ तक)
मूल तथा अनुवाद सहित
श्रीअरविन्द की अंग्रेजी टीका के हिन्दी अनुवाद एवं व्याख्या सहित
अंग्रेजी टीका का संपादन
स्व. श्री परमेश्वरी प्रसाद खेतान
हिन्दी व्याख्या
चन्द्र प्रकाश खेतान
हिन्दी अनुवाद व व्याख्या संपादन
पंकज बगड़िया
श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट
झुंझनू, राजस्थान
© श्रीअरविन्द आश्रम ट्रस्ट, २०१९
प्रकाशक
श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट
श्री अरविन्द दिव्य जीवन आश्रम
खेतान मोहल्ला
झून्झून-३३३००१, राजस्थान
URL: www.sadlec.org
www.aurokart.com
मुद्रक :-
श्रीअरविन्द आश्रम प्रेस
पुदुच्चेरी
भगवान् श्रीकृष्ण को समर्पित
जिनकी कृपा से हमें
श्रीअरविन्द व श्रीमाँ के चरण कमलों की
शरण प्राप्त हुई है।
संपादकीय नोट
यह पुस्तक स्वर्गीय श्री परमेश्वरी प्रसाद खेतान द्वारा संपादित अंग्रेजी पुस्तक 'द भगवद् गीता' के हिन्दी रूपांतर के आधार पर श्रीअरविन्द दिव्य जीवन शिक्षा केन्द्र में हुए अध्ययन सत्रों में साधकों के बीच हुई चर्चा-परिचर्चा, सहज अंतःस्फूणा तथा श्री चन्द्र प्रकाश जी खेतान के निजी आध्यात्मिक अनुभवों आदि के माध्यम से हुई श्रीअरविन्द व श्रीमाँ के मूल शब्दों की व्याख्या का अभिलेख है। सत्रों के ध्वनिलेखों को भाषा में ढालने और उनकी एडिटिंग (संपादन), संशोधन आदि का कार्य सुश्री सुमन शर्मा व श्री दीपक तुलस्यान की सहायता से मेरे द्वारा किया गया है। अनेक स्थानों पर चर्चा-परिचर्चा के दौरान श्रीमाँ-श्रीअरविन्द तथा योगी श्रीकृष्णप्रेम के जिन संदर्भों का हवाला दिया गया था उन्हें यहाँ मूल रूप से सम्मिलित कर लिया गया है जो कि पाठक के लिये पूरे विषय को अधिक स्पष्ट, सुगम और प्रभावी बना देते हैं। व्याख्या को मूल से पृथक् करने के लिए तिरछे अक्षरों (italics) का प्रयोग किया गया है। प्रथम भाग में गीता के प्रथम सात अध्यायों को सम्मिलित किया गया है और दूसरे भाग में शेष ग्यारह अध्यायों को सम्मिलित किया गया है।
पुस्तक में प्रस्तुत गीता पर टीका श्रीमाँ की कृतियों से लिये कुछ संदर्भों को छोड़कर शेष श्रीअरविन्द के शब्दों में है जिनकी संदर्भ सूची अंत में दी जा रही है। विचार में निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर मूल संपादक श्री परमेश्वरी प्रसाद खेतान द्वारा कुछ शब्द या वाक्यांश जोड़े गए हैं जिन्हें वर्गाकार कोष्ठक में दिखाया गया है।
मूल संस्कृत श्लोकों का अनुवाद तथा पुस्तक में दिये गये शीर्षक श्रीअरविन्द की पुस्तक 'ऐसेज ऑन द गीता' पर आधारित हैं। अध्यायों के परंपरागत शीर्षक प्रत्येक अध्याय के अंत में दिये गये हैं। हासिये में दी गई संख्याएँ गीता के अध्याय व श्लोक संख्या को दर्शाती हैं।
जैसा कि श्रीमाँ ने कहा "श्रीअरविन्द गीता के संदेश को उस महान् आध्यात्मिक गति का आधार मानते हैं जो मानवजाति को अधिकाधिक उसकी मुक्ति की ओर, अर्थात् मिथ्यात्व और अज्ञान से निकलकर सत्य की ओर ले गई है, और आगे भी ले जाएगी। अपने प्रथम प्राकट्य के समय से हो गीता का अतिविशाल आध्यात्मिक प्रभाव रहा है; परंतु जो नवीन व्याख्या श्रीअरविन्द ने उसे प्रदान की है, उसके साथ ही उसकी प्रभावशालिता अत्यधिक बढ़ गई है और निर्णायक बन गई है।"
वर्ष १९९२ में अपने प्रथम संस्करण के समय से ही स्व. श्री परमेश्वरी प्रसाद खेतान द्वारा संपादित 'द भगवद्गीता' पुस्तक को पाठकों द्वारा खूब सराहा गया है। श्रीअरविन्द की अद्भुत टीका के तीसरे संस्करण के ऊपर अब इस व्याख्या के आने से हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक श्रीअरविन्द व श्रीमाँ के आलोक में गीता को समझने, उसे व्यावहारिक रूप से जीवन में उतारने में पाठकों के लिए और अधिक सहायक सिद्ध होगी।
- पंकज बगड़िया
विषय-सूची
I.अवतार-तत्त्व की सम्भावना, उसका उद्देश्य और उसकी प्रक्रिया
II. निर्वाण तथा संसार में कर्म
निर्वाण, समता एवं संसार में कर्म
प्रस्तावना
I. अन्वेषण का भाव
...वेद, उपनिषद् अथवा गीता जैसे किसी प्राचीन सग्रंथ के अन्वेषण में आरंभ में ही ठीक-ठीक यह स्पष्ट कर देना बहुत उपयोगी होगा कि हम किस विशिष्ट भाव से इस अन्वेषण में प्रवृत्त हो रहे हैं और वास्तव में हम क्या समझते हैं कि इससे वह कौनसी चीज प्राप्त करेंगे जो मानवजाति और उसके भविष्य के लिए महत्त्व की होगी। सर्वप्रथम, निःसंदेह हम एक ऐसे परम सत्य की खोज कर रहे हैं जो एकमेव व सनातन हो, जिससे अन्य सभी सत्य प्रादुर्भूत होते हों, जिसके प्रकाश से अन्य सभी सत्य ज्ञान की योजना में अपना उचित स्थान, अपनी व्याख्या अथवा निरूपण तथा अपना परस्पर संबंध पाते हैं। परंतु ठीक इसी कारण वह परम सत्य किसी एक तीक्ष्ण या एकांगी सूत्र के अंदर बंद नहीं किया जा सकता, कदाचित् ही वह हमें समग्रता में तथा संपूर्ण आशय सहित किसी एक दर्शन में या किसी एक सग्रंथ में, या फिर किसी एक गुरु, मनीषी, पैगम्बर या अवतार के मुख से पूर्ण रूप में तथा सदा के लिए पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ मिले। और यदि उस सत्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण या भाव उसे छोड़कर अन्य प्रणालियों अथवा पद्धतियों में निहित सत्यों के असहिष्णु बहिष्कार को आवश्यक बताता हो तब भी इसका अर्थ है कि वह सत्य अपनी समग्रता में हमारे द्वारा खोजा नहीं गया है; क्योंकि जब हम आवेश में आकर अथवा तीक्ष्ण रूप से निषेध करते हैं तो सीधे-सीधे इसका अर्थ होता है कि इस सत्य को समझने अथवा सराहने में तथा इसे निरूपित करने में हम समर्थ नहीं हैं। दूसरे, यद्यपि यह सत्य एकमेव तथा सनातन है, तो भी यह अपने-आप को काल में और मनुष्य की मन-बुद्धि द्वारा अभिव्यक्त करता है; अतः प्रत्येक सग्रंथ में आवश्यक रूप से दो तत्त्व होते हैं, एक अस्थायी या सामयिक, नश्वर तथा उस देश और काल विशेष के विचारों से संबद्ध जिसमें वह उत्पन्न हुआ था, और दूसरा तत्त्व होता है सनातन व अविनश्वर तथा सभी कालों व देशों में प्रयोज्य या व्यवहार्य। इसके अतिरिक्त परम सत्य की अभिव्यक्ति अथवा वर्णन में उसे जो वर्तमान रूप दिया जाता है, जिस पद्धति तथा योजना से, जिस तात्त्विक व बौद्धिक साँचे में ढालकर और जिस विशिष्ट वाक्य रचना का प्रयोग कर उसको अभिव्यक्ति की जाती है वे सब अधिकांशतः काल के परिवर्तनों के अधीन होते हैं और इस कारण (कालांतर से) वैसी ही शक्ति नहीं रख पाते; क्योंकि मानव-बुद्धि सदा अपने-आप में बदलाव लाती रहती है; निरंतर ही विभाजन करती और संयोजन करती हुई यह निरंतर ही अपने विभाजनों को बदलने और अपने समन्वयों को नए क्रम से रखने को बाध्य होती है; यह नवीन वाक्य-रचनाओं अथवा अभिव्यक्तियों तथा प्रतीकों हेतु पुरातन का त्याग करती जाती है, या फिर यदि वह पुरातन प्रयोगों का पुनः उपयोग करती भी है तो भी उसके संकेतार्थ या गूढार्थ को या कम-से-कम उसकी वास्तविक अंतर्वस्तु तथा अर्थ-संगतियों को इस प्रकार इतना बदल देती है कि हम इस प्रकार की प्राचीन पुस्तक को पढ़ते समय इस विषय में कभी भी सर्वथा सुनिश्चित नहीं हो सकते कि उसे हम उसी आशय और भाव में समझ पा रहें हैं जैसा आशय व भाव वह पुस्तक अपने समकालीन लोगों के लिए रखती थी। अतः ऐसे सग्रंथ में जो तत्त्व चिरंतन महत्त्व का है वह वह तत्त्व है जो सार्वलौकिक होने के साथ ही अनुभूत किया गया हो, जीया गया हो और बौद्धिक दृष्टि की अपेक्षा उच्चतर दृष्टि से देखा गया हो।
भगवान् का पूर्ण सत्य तो कभी अभिव्यक्त किया जा ही नहीं सकता। इसलिए जब यह अभिव्यक्ति में आता है तो सीमित हो जाता है। कोई अनुभव, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, बहुत आन्तरात्मिक जगत् का ही क्यों न हो, तो भी उसके लिए हम यह नहीं कह सकते कि वह चरम अनुभव है। अवश्य ही वह बहुत गंभीर हो सकता है, सत्य हो सकता है। पहली चीज तो यह है कि भगवान् के सत्य की पूर्ण अभिव्यंजना हो ही नहीं सकती। परंतु जगज्जननी ऐसी ही असंभव चीज को साधित करने का प्रयत्न कर रही हैं अन्यथा ये ऐसे ब्रह्माण्ड अभिव्यक्ति में आते ही नहीं। यदि व्यक्ति का उस परम् का अनुभव बहुत गहन भी हो, तो किसी अर्थ में वह उसे समझ तो सकता है, पर जब वह उसकी अभिव्यक्ति करना चाहता है तो जो मानसिक चेतना है, जो बुद्धि है, उसमें वह पाता है कि वास्तव में इसे समुचित रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारे वैदिक ऋषियों ने पाया कि तर्कबुद्धि की भाषा में इसे अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकात्मक भाषा को ही उन्होंने सबसे अच्छा माध्यम पाया। यदि व्यक्ति अंतर्बोधात्मक चेतना में हो तो वे प्रतीक उसके लिए जीवित-जागृत होंगे, सजीव होंगे। उसके लिए वे कोई मृत पर्यायवाची नहीं होगे, जैसे कि एक पहाड़ का अर्थ अभीप्सा से लगा लिया जाए, या फिर नदी का अर्थ चेतना से लगा लिया जाए। ऐसे प्रतीकों की भाषा में हम उस सत्य को थोड़ा-बहुत अभिव्यक्त कर सकते हैं। वेदों में जो अभिव्यक्ति हुई है वह इसी प्रकार की है। परंतु अब चूंकि हम उन प्रतीकों के पीछे के गूढ़ार्थ तक नहीं जा पाते इसलिए उनमें निहित सत्य हमारे लिए अगम हो गया है। उपनिषदों में उसे कुछ अधिक मानसिक भाषा में अभिव्यक्त किया गया है, गीता उनसे भी अधिक मानसिक भाषा में उसका निरूपण कर रही है। पर यहाँ भी जो निरूपण-पद्धति है, जो प्रतीक प्रयोग में लाए गए हैं, वे उस समय अभिव्यक्ति के लिए जो उचित महसूस हुए उस अनुसार प्रयोग में लाए गए हैं। परंतु यह सब होने के बावजूद भी जब उस सत्य की अभिव्यक्ति होती है, तब यदि हममें क्षमता हो, अंतर्ज्ञान हो, आंतरिक समझ हो तो हम शब्दों के परे भी उस सत्य को पकड़ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तब शब्द हमारे लिए केवल एक पारदर्शी पर्दा-मात्र रह जाते हैं। इसी कारण हमारे ऋषियों ने जिस प्रकार की शब्दाभिव्यक्ति की है, जिस रीति से उन्होंने उस सत्य की अभिव्यक्ति की है वह हमें उस सत्य तक पहुँचने में अधिक रोकती नहीं है और हमें उस सत्य के दर्शन हो जाते हैं। जिस पुस्तक में वह पर्दा बहुत झीना होता है, पारदर्शी होता है उसमें उस सत्य को देखना अधिक आसान होता है। और गीता ऐसी ही पुस्तकों में से एक है जिसमें उस सत्य की अभिव्यक्ति बड़ी अच्छी तरह से हुई है और आवरण बहुत ही कम है, इसलिए यह शाश्वत रहती है क्योंकि कोई भी मनुष्य जो थोड़ी-बहुत भी गहराई में स्थित है उसके लिए इसमें से कुछ ग्रहण करना अधिक आसान है। यदि कोई अधिक गहराई में निवास न भी कर रहा हो तो भी वह इससे इतना तो अवश्य ही ग्रहण कर सकेगा जो उसके लिए उपयोगी होगा। इसलिए गीता की यह विशिष्टता है कि इसमें सबके लिए कुछ-न-कुछ अवश्य ही मिल जाता है। यह जो शाब्दिक अभिव्यक्ति का बाहरी तत्त्व है उसी पर अधिक आग्रह रखने की अपेक्षा हम उससे आगे जा सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि गीता जो बता रही है हम उससे शुरू करें और उससे भी परे चले जाएँ।
श्रीअरविन्द की 'एसेज ऑन द गीता' की सारी टीका यही तो दर्शाती है। ऐसा संभव है कि गीतोपदेश में जिन चीजों के बारे में स्वयं श्रीकृष्ण भी बोलने में सचेतन न रहे हों, चूंकि तब वे योगारूढ़ थे और उनके द्वारा वह उपदेश प्रवाहित हो रहा था, उसे भी श्रीअरविन्द अब सामने ला रहे हों। ऐसा नहीं है कि जो सत्य उसमें निहित हैं वे उस अभिव्यक्ति से सीमित हैं। हम उससे आगे जा सकते हैं, कितना भी आगे जा सकते हैं। वेदों की विवेचना में यह संभव है कि वैदिक ऋषि जितना समझते थे हम उससे भी आगे जा सकते हैं क्योंकि आखिर यही तो इस सत्य की विलक्षणता है। हमारी चेतना के द्वारा यह काम किया जाना संभव है। इसलिए ऐसी पुस्तकें अपने-आप में आध्यात्मिक ऊर्जा-स्रोत के समान होती हैं। जिस प्रकार चित्र, चित्रकारियाँ, स्थापत्य आदि भी ऊर्जा-स्रोत हो सकते हैं जो किसी पात्र के समक्ष किसी गहन अंतर्दर्शन को प्रकट कर सकते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार का माध्यम बन सकते हैं, उसी प्रकार ये सद्ग्रंथ हैं। गीता भी इसी प्रकार की एक पुस्तक है। इसलिए श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि यह जानने का महत्त्व कम है कि तात्कालिक लोगों ने इसे किस प्रकार समझा था। हमारे लिए आवश्यक यह है कि हम स्वयं इसे जानें और साथ ही यह जानें कि इसे अभिव्यक्त कैसे करें ताकि अधिक-से-अधिक लोग उससे जुड़कर, इसके ज्ञान पर सवार होकर उत्तरोत्तर आरोहण कर सकें। इसी प्रयोजन से श्रीअरविन्द ने 'गीता प्रबंध' लिखी। गीता में यदि उन्हें वह सूत्र न मिला होता, प्रचुर रूप से वह शाश्वत् तत्त्व न मिला होता, जो आज भी उतना ही नूतन तथा सत्य है - चूँकि गीता की नवीनता जितनी अपनी शुरुआत में थी उतनी ही आज भी है तो वे कहते हैं कि इसमें वे अपना समय नष्ट नहीं करते। जो भी भगवान् के और जगत् के रहस्य को जानना चाहता है वह गीता को अनदेखा नहीं कर सकता। सभी वाद-विवादियों की इस विषय में मत-भिन्नता है कि श्रीकृष्ण के कथन का तात्पर्य क्या था। परन्तु इसकी बजाय देखना तो यह चाहिये कि आज के समय में उसका अर्थ क्या हो सकता है। अभिव्यक्ति में तो वह सत्य पूर्णतः आ ही नहीं सकता। और यदि कहीं किसी ने उसे अभिव्यक्त किया भी हो तो वह अंतिम नहीं हो सकता। हमेशा ही व्यक्ति उससे अधिक ऊँचाई पर जा सकता है तथा उसी चीज की अभिव्यक्ति को और अधिक समृद्ध बना सकता है। जैसे कि बुद्ध की प्रतिमा के चेहरे के भाव को देखकर योगी श्रीकृष्णप्रेम ने कहा कि 'अवश्य ही वैसा भाव कहीं विद्यमान होना चाहिये अन्यथा वह अभिव्यक्त ही कैसे हो पाता।' आवश्यक नहीं कि स्वयं वह मूर्तिकार भी उस भाव के विषय में सचेतन रहा हो परंतु अवश्य ही कोई दूसरी शक्ति उसके हाथों को काम में ले रही थी क्योंकि (जैसा कि श्रीअरविन्द अपने 'सावित्री' महाकाव्य में लिखते हैं) 'अदर्शक हाथ अदृष्ट की आज्ञा पालन करते हैं' (p. 460)। बुद्ध के चेहरे पर जो करुणा का भाव अभिव्यक्त हुआ है, उनकी आँखों में जो शांति है, वह कहीं न कहीं तो अवश्य ही विद्यमान है और उन्हें उसी की खोज करनी है। उन्होंने कहा कि उस मूर्ति ने उनके समक्ष जिन चीजों को प्रकट किया वैसा तो कदाचित् वे पाली में सारे बौद्ध साहित्य का अध्ययन कर के भी नहीं समझे होंगे।' अतः परमात्मा का सत्य एक ऐसी विलक्षण चीज है जिस पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। अपने-अपने दृष्टिकोण से सभी उसे भिन्न-भिन्न रूप से समझते हैं। उसे हम अपने मन में, प्राण में, भौतिक सत्ता में जिस भी प्रकार से समझेंगे उसी प्रकार से उसे अभिव्यक्त करेंगे। और चूंकि उस वैयक्तिक अभिव्यक्ति का इतना भारी मूल्य है इसीलिए सृष्टि इतनी जटिल है। यदि मनुष्य, प्राणी, पशु-पक्षी, पत्थर आदि सभी अपने-अपने तरीके से परमात्मा के निरपेक्ष सत्य को अभिव्यक्त न कर रहे होते तो वे अस्तित्व में आ ही नहीं सकते थे। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता क्योंकि असत्य का अस्तित्वमान होना तो एक अतात्त्विक बात है। सभी चीजें सत्य के किसी-न-किसी पहलू को अवश्य ही अभिव्यक्त करती हैं। एक बार जब यदि हमें इस बात का बोध हो जाए कि सभी अपने-अपने तरीके से उस सत्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो हम घोर संकीर्णता से कुछ बच सकते हैं और चीजों के प्रति एक अधिक सहिष्णु और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना सकते हैं। प्रस्तुत प्रस्तावना में श्रीअरविन्द ने इस बिंदु को बहुत सुंदर ढंग से रखा है कि सग्रंथों के प्रति उचित दृष्टिकोण क्या होना चाहिये। अन्यथा व्यक्ति इनके विषय में अंध श्रद्धा रखने का दकियानूसी दृष्टिकोण अपना लेता है और हठपूर्वक इस पर आग्रह करने लगता है कि पुस्तक में इसने या उसने वैसी ही बात कही है जैसा उसने स्वयं समझा है। परंतु इसमें व्यक्ति को समझना होगा कि समस्या उस कही हुई बात में नहीं अपितु वह उसे जिस रूप में समझता है उसमें है, क्योंकि जो कहा गया है उसके बारे में वह निश्चित कैसे हो सकता है कि वह उसे वैसा ही समझ रहा है। और फिर केवल वही अन्तिम सत्य हो यह भी आवश्यक नहीं है।
अतः गीता के उस बिल्कुल सटीक तात्त्विक गूढार्थ को वैसे ही जानना जैसा कि उस समय के लोगों द्वारा समझा गया था, - यदि ऐसा सही-सही करना संभव भी होता - तो भी इसे मैं गौण महत्त्व का मानता हूँ। और यह संभव भी नहीं है जैसा कि गीता पर लिखे गए और अभी भी लिखे जा रहे मूलभाष्यों की परस्पर मत-भिन्त्रता से स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि ये सभी एक दूसरे से असहमत होने में ही एकमत हैं, प्रत्येक ही गीता में अपनी ही तत्त्वज्ञान की पद्धति तथा धार्मिक विचारधारा खोज निकालता है और यहाँ तक कि अत्यंत श्रमसाध्य निष्पक्ष विद्वत्ता तथा भारतीय दर्शन के ऐतिहासिक विकासक्रम के विषय में अत्यंत प्रकाशमान सिद्धांत भी हमें इस अपरिहार्य भूल से नहीं बचा सकते। परंतु लाभकारी रूप से जो हम कर सकते हैं वह यह है कि गीता में निहित उन यथार्थ जीवंत सत्यों को खोजें, भले ही उनके तत्त्वविज्ञानसंबंधी रूप जो भी हों, और इसमें से वह तत्त्व निकालें जो हमें अथवा व्यापक रूप से संसार को सहायता पहुँचा सकता है और फिर यथासंभव ऐसे अत्यंत स्वाभाविक तथा जीवंत रूप व शब्द-अभिव्यक्ति में उसे व्यक्त करें जो हमारी वर्तमान मनुष्यजाति की मानसिकता के अनुरूप तथा उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो... यदि हम इस महान् सग्रंथ के भाव में अपने-आप को तल्लीन कर दें और विशेषकर यदि हमने उस भाव में जीने का प्रयास किया हो तो हम उसके अंदर उतना यथार्थ सत्य प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं जितने को ग्रहण करने के हम पात्र हैं और साथ ही व्यक्तिगत तौर पर इससे हम उतना आध्यात्मिक प्रभाव और वास्तविक सहायता प्राप्त कर सकते हैं जितना इसमें से प्राप्त करना हमारे लिए अभिप्रेत था। और, अंततः, यही देने के लिए तो ये सग्रंथ लिखे गए थे; शेष सब केवल शास्त्रीय वाद-विवाद और धार्मिक मत-मतांतर है। केवल वे ही सद्ग्रंथ, धर्म तथा दर्शन मनुष्यजाति के लिए जीवंत महत्त्व के बने रहते हैं जो कि इस प्रकार सतत् ही नवीकृत हो सकते हों, पुनः जीये जा सकते हों, तथा उनमें निहित सनातन सत्य के तत्त्व को सतत् ही नए रूपों में गढ़कर एक विकसनशील मनुष्यजाति के अंतःविचार तथा आध्यात्मिक अनुभव में विकसित किया जा सकता हो। शेष सब अतीत के स्मारकों के रूप में बचे रहते हैं परंतु उनमें भविष्य के लिए कोई यथार्थ शक्ति या सजीव प्रेरणा नहीं होती।
इस अंश में जो नया बिंदु है वह यह है कि, हमारे वैदिक ऋषियों ने जिन प्रतीकों में अभिव्यक्ति की है वे प्रतीक नित-नूतन, चिन्मय और जीवंत हैं। उन प्रतीकों की व्याख्या हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकते हैं और उस रूप में उन्हें समझ सकते हैं। पर जब वह अभिव्यक्ति ऐसे शब्दों में, ऐसे प्रतीकों में होती है जो बहुत अधूरे हैं, जैसे कि अमूर्त मानसिक भाषा या मानसिक प्रतीक, तब फिर समय के साथ वे प्रासंगिक नहीं रह पाते, और अपने को देश-काल के अनुसार नमनीय न रह पाने के कारण क्षणिक या अस्थायी विषय बनकर रह जाते हैं। कितनी ही बौद्धिक पुस्तकें आती हैं जो कुछ समय प्रचलन में रहने के बाद प्रचलन से बाहर हो जाती हैं। कुछ में यदि कुछ अधिक अंतर्वस्तु होती है तो वे कुछ अधिक समय तक टिक जाती हैं। जहाँ सत्य को शक्तिशाली रूप से अभिव्यक्त किया हुआ नहीं होता, जीवंत प्रतीक की भाषा के अन्दर यदि सत्य की संवेदनशील अभिव्यक्ति नहीं हुई होती या फिर यदि व्यक्ति के अन्दर धर्मांधता है जिस कारण वह उस पर आवश्यकता से ज्यादा या कम महत्त्व देता है तो वे अभिव्यक्तियाँ अपना मूल्य खो बैठती हैं, और ऐसी पुस्तकें अपने बने रहने की शक्ति खो बैठती हैं। हो सकता है व्यक्ति ने सत्य के कुछ अंश को देखा हो पर उसकी अभिव्यक्ति बड़ी भौंडी होने के कारण वह निरंतर नहीं रह पाती। परंतु इस सब के साथ ही साथ यह भी एक तथ्य है कि जिन सत्यों को बहुत गहराई में देखा जाता है वे अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति अपने साथ ले आते हैं, जैसा कि गीता में हुआ है, वेदों में हुआ है। ये पुस्तकें सदा नूतन बनी रहती हैं। क्योंकि उनके अनुभव को सदा ही अनुभूति में पुनः जीया जा सकता है। और फिर गीता के कुछ तत्त्व जो देश-काल मर्यादित प्रतीत होते हैं - जैसे कि जाति-प्रथा, यज्ञ-अनुष्ठान आदि तात्कालिक विषय- उन्हें भी श्रीअरविन्द कहते हैं कि जिस निहित गहरे अर्थ में गीता उनका प्रयोग करती है उस रूप में ले लिया जाए तो उनके अर्थ की वह सीमितता भी लुप्त हो जाती है। जैसे कि गीता में यज्ञ का जो विचार अंतर्निहित है तीसरे अध्याय में तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिल्कुल ही अपूर्ण और अपरिपक्व है, मानो वह समय-विशेष और समुदाय विशेष के लिए ही प्रयोजनीय हो, परन्तु चौथे अध्याय में गीता ने उस सारी सीमितता को यह कह कर तोड़ दिया कि ब्रह्म ही यज्ञ है, ब्रह्म ही अभीप्सा है, सब कर्म ब्रह्म ही हैं। इसलिए हर प्रतीक को यदि हम गहराई में देखें तो वह उस देश और काल से सीमित नहीं रहता अपितु शाश्वत रूप ग्रहण कर लेता है। अतः गीता में ऐसा बहुत ही कम है जो हमें परिसीमित करता हो। इसीलिए यह बहुत मूल्यवान् है।
(iv.24)
गीता में ऐसा विषय बहुत ही कम है जो देश से सीमित और सामयिक अथवा अस्थायी हो और इसका भाव और विचारधारा इतनी उदार, गंभीर और व्यापक है कि उस थोड़े बहुत को भी सरलतापूर्वक, इसकी शिक्षा का जरा भी हास या अतिक्रम किये बिना, व्यापक रूप दिया जा सकता है; यही नहीं, उसे देश या काल से संबद्ध रखने की बजाय ऐसा व्यापक रूप देने पर उसकी शिक्षा की गहराई, उसके सत्य और उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। वास्तव में, स्वयं गीता ही बारंबार उस व्यापक रूप का संकेत करती है जो किसी विचार को दिया जा सकता है भले ही वह विचार अपने-आप में देशकालमर्यादित हो। जैसे कि 'यज्ञ' संबंधी प्राचीन भारतीय विधि और विचार को गीता देवताओं और मनुष्यों के पारस्परिक आदान-प्रदानस्वरूप मानती है - जबकि यह विधि और भाव स्वयं भारतवर्ष में ही दीर्घ काल से लगभग लुप्त हो गए हैं और सर्वसाधारण मानव-मन को और अधिक यथार्थ प्रतीत नहीं होते; परन्तु गीता में इस 'यज्ञ' शब्द को हम इतना संपूर्ण रूप से सूक्ष्म, आलंकारिक और प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया पाते हैं तथा देवता-संबंधी धारणा देशकालमर्यादा और किंवदंती से न के बराबर ही बँधी हुई अथवा इतनी मुक्त और इतनी पूर्ण रूप से सार्वभौमिक और दार्शनिक है कि हम यज्ञ और देवता दोनों को मनोविज्ञान और प्रकृति के साधारण विधान के व्यावहारिक तथ्य के रूप में सहज ही ग्रहण कर सकते हैं और इन्हें, प्राणियों में परस्पर होनेवाले आदान-प्रदान, एक-दूसरे के हितार्थ होनेवाले बलिदान और आत्मदान के विषय में जो आधुनिक विचार हैं, उन पर इस तरह प्रयुक्त कर सकते हैं कि इनके अर्थ और भी अधिक उदार और गम्भीर हो जाएँ, ये अधिक आध्यात्मिक स्वरूप वाले और गंभीरतर तथा अधिक विस्तीर्ण सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएँ। इसी प्रकार शास्त्र-सम्मत कर्म करने का विचार, समाज की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, चारों वर्णों की परस्पर स्थिति का, या दूसरों की तुलना में शूद्रों और स्त्रियों के आध्यात्मिक अनधिकार का उल्लेख, ये सब प्रथम दृष्ट्या देश या काल-विशेष से संबद्ध प्रतीत होते हैं और यदि इनके शाब्दिक अर्थ पर ही अतिशय बल दिया जाए तो कम-से-कम ये गीता की शिक्षा को उतने अंश में संकीर्ण बना देते हैं, गीता को उसके उपदेश की व्यापकता और आध्यात्मिक गंभीरता से वंचित कर देते हैं और, अधिक व्यापक रूप से, समस्त मनुष्य जाति के लिए उसकी प्रामाणिकता को सीमित कर देते हैं। परन्तु यदि हम इसके पीछे के आन्तरिक भाव और अर्थ को देखें, न कि केवल देश-विशिष्ट नाम और काल-विशिष्ट रूप को, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी अर्थ गहरा और यथार्थ है और इसका आन्तरिक भाव दार्शनिक, आध्यात्मिक और सार्वभौमिक है। शास्त्र शब्द से प्रतीत होता है कि गीता का तात्पर्य उस विधान से है जिसे मनुष्य जाति ने स्वयं के ऊपर उस प्राकृत असंस्कृत मनुष्य के निरे अहंभावापन्न कर्म के स्थान पर, तथा अपनी वासनाओं की तृप्ति को ही अपने जीवन का मानक और उद्देश्य बना लेने की प्रवृत्ति पर एक अंकुश के रूप में आरोपित किया है। ऐसे ही हम देखते हैं कि समाज को चातुर्वर्ण्य व्यवस्था भी एक आध्यात्मिक तथ्य का ही महज एक स्थूल रूप है, जो स्वयं उस स्थूल रूप से स्वतंत्र है; यह स्वभाव नियत कर्म की उस अवधारणा पर आश्रित है जिसमें कि कर्म, उस कर्ता के स्वभाव की सम्यक् क्रमानुगत अभिव्यक्ति के अनुसार निष्पादित हों, और वह स्वभाव नैसर्गिक गुण और आत्माभिव्यक्तिकारी वृत्ति के अनुसार उसके जीवन की धारा और क्षेत्र को निर्धारित करे। चूँकि गीता अपने अत्यंत स्थानिक और सामयिक दृष्टांतों को इसी (गंभीर और व्यापक) भाव से प्रस्तुत या विकसित करती है, अतः सर्वत्र ही हमारा इसी सिद्धांत का अनुसरण करना और सर्वत्र ही उस गंभीरतर सामान्य सत्य को ढूँढ़ना औचित्यपूर्ण ही होगा जो कि अवश्य ही उन सब प्रथम दृष्ट्या दिखने में स्थानिक और सामयिक बातों के पीछे छिपा होता है। क्योंकि हम सदा ही ऐसा पाएँगे कि वह गंभीरतर सत्य और सिद्धांत चिंतन के स्वभाव मात्र में ही तब भी निहित होता है जब वह स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया होता है।
और न ही हमें उन दर्शनसंबंधी मतों या धर्म संबंधी मान्यताओं के साथ अन्य किसी भाव से व्यवहार करना चाहिए, जो कि गीता में सामयिक दार्शनिक शब्दों के या धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग के कारण प्रवेश कर जाते हैं या फिर किसी प्रकार इससे संबद्ध हो गए हैं... न ही हमें उन मत-मतांतरों पर चर्चा करने की आवश्यकता है जो गीता को किसी धार्मिक संप्रदाय या परंपरा-विशेष का फल मानते हैं। गीता का उद्गम जो भी रहा हो, परंतु इसका उपदेश सार्वभौमिक अथवा व्यापक है।
गीता की दार्शनिक पद्धति, इसमें सत्य का जो व्यवस्थापनक्रम है वह इसके उपदेश का वह भाग नहीं है जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण, गहन तथा चिरस्थायी हो; किन्तु इसकी रचना का अधिकांश विषय, इसके सांकेतिक और मर्मस्पर्शी प्रधान विचार जो इस ग्रंथ के जटिल सामंजस्य में पिरोये गये हैं, वे चिरंतन रूप से मूल्यवान् तथा प्रामाणिक हैं, क्योंकि, वे महज एक दार्शनिक बुद्धि के चमकदार विचार या चकित करनेवाली परिकल्पनाएँ नहीं हैं, अपितु आध्यात्मिक अनुभव के चिरस्थायी सत्य हैं, हमारी उच्चतम अध्यात्मपरक संभावनाओं के प्रमाणयोग्य तथ्य हैं, जिन्हें इस जगत् के रहस्य की तह तक पहुँचने के प्रयास में कदापि उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इसकी विवेचन पद्धति जो भी हो, जैसा कि भाष्यकार प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु इसका गठन न तो किसी दार्शनिक मत विशेष का समर्थन करने हेतु या फिर किसी एक विशिष्ट योग पद्धति के दावों को ही मुख्य रूप से प्रतिपादित करने हेतु हुआ है और न ही ऐसा करने के लिए यह अभिप्रेत या नियत है। गीता की भाषा, विचार की संरचना, विविध विचारों का इसमें संयोजन और उनका संतुलन, न तो किसी सांप्रदायिक आचार्य की मनोवृत्ति से संबंध रखते हैं, और न ही वह किसी ऐसे सख्त विश्लेषणात्मक तर्कशास्त्री की प्रकृति से जो सत्य के किसी एक पहलू को काट-छाँटकर बाकी सबको अलग कर देने की प्रवृत्ति रखती हो, अपितु इसकी अपेक्षा इसमें तो विचारों की एक विस्तृत, तरंगित और सर्वालिंगनकारी गति है जो एक विशाल समन्वयात्मक बुद्धि और सुसंपन्न समन्वयात्मक अनुभूति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। यह उन महान् समन्वयों में से एक है जिनकी सृष्टि करने में भारत की आध्यात्मिकता उतनी ही समृद्ध रही है जितनी कि ज्ञान की उन अत्यंत प्रगाढ़ और अनन्य क्रियाओं तथा धार्मिक साक्षात्कारों की सृष्टि करने में, जो परम एकाग्रता के साथ किसी एक ही सूत्र को अथवा एक ही मार्ग को उसकी पराकाष्ठा तक अनुसरण करते हैं। । गीता की विचारधारा] काटकर पृथक् पृथक् नहीं करती, अपितु सामंजस्य और ऐक्य साधित करती है।
गीता का विचार अथवा सिद्धांत शुद्ध रूप से केवल अद्वैतवाद नहीं है यद्यपि इसकी दृष्टि में एक ही अव्यय, विशुद्ध, सनातन आत्मतत्त्व अखिल ब्रह्माण्ड की स्थिति का आश्रय है; न मायावाद ही है यद्यपि यह सृष्ट जगत् में त्रिगुणात्मिका प्रकृति की सर्वव्यापी माया की चर्चा करती है; न यह विशिष्टाद्वैत ही है यद्यपि यह उस एकमेवाद्वितीय परब्रह्म में उसकी सनातन परा प्रकृति को स्थित बताती है जो कि जीव के रूप में अभिव्यक्त होती है और साथ ही (गीता) आध्यात्मिक चेतना की परम स्थिति के रूप में परब्रह्म में लय की अपेक्षा उसमें निवास करने पर ही अत्यधिक बल देती है; न यह सांख्य ही है यद्यपि यह सृष्ट जगत् की व्याख्या प्रकृति-पुरुष के द्विविध तत्त्व के द्वारा करती है; न यह वैष्णव ईश्वरवाद ही है यद्यपि यह पुराण प्रतिपादित श्रीविष्णु के ही अवतारस्वरूप श्रीकृष्ण को हमारे समक्ष परमाराध्य देवाधिदेव के रूप में निरूपित करती है, और न ही इन भूतेश में जो कि जगत्पति तथा समस्त प्राणियों के परम सखा हैं तथा उस अनिर्देश्य निर्विशेष ब्रह्म में कोई तात्त्विक भेद करती है और न ही उस ब्रह्म के पद में इन कृष्ण से कोई वास्तविक श्रेष्ठता को ही स्वीकार करती है। गीता के पूर्व उपनिषदों में जैसा समन्वय हुआ है वैसा ही गीता का समन्वय है जो कि आध्यात्मिक होने के साथ-ही-साथ बौद्धिक भी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे किसी भी अनुदार मत को परिवर्जित कर देता है जो इसकी सार्वलौकिक व्यापकता को क्षति पहुँचाए। इसका उद्देश्य उन खण्डनात्मक भाष्यकारों के उद्देश्य से ठीक विपरीत है जिन्होंने इस सद्ग्रंथ को सर्वाधिक प्रामाणिक तीन वेदान्तिक ग्रंथों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित पाया और इसे स्वमत के मंडन तथा अन्य मतों और संप्रदायों के खण्डन के लिए शस्त्र के रूप में प्रयुक्त करने का प्रयास किया। गीता कोई तर्कशास्त्रीय युद्ध का अत्र नहीं है; यह एक ऐसा महाद्वार है जो समस्त आध्यात्मिक सत्य और अनुभूति के जगत् की ओर खुलता है और जो झाँकी यह हमें प्रदान करता है वह उस परम दिव्य धाम के सभी क्षेत्रों को अपने में समाविष्ट कर लेती है। गीता इन क्षेत्रों को योजनाबद्ध तो करती है, पर कहीं भी यह [एक से दूसरे क्षेत्र को] विच्छिन्न नहीं करती, न किसी प्रकार की दीवारें या घेरा खड़ा करती है जो कि हमारी दृष्टि को परिरुद्ध कर दे।
मानव-मन सदा आगे की ही ओर बढ़ता है, अपने दृष्टिकोण को बदलता तथा अपने विचार के विषयों को विस्तृत करता है, और इन परिवर्तनों का परिणाम होता है चिंतन की पुरातन प्रणालियों को अप्रचलित या लुप्तप्राय बना देना अथवा, जब उन्हें सुरक्षित रखा भी जाए तब भी, उन्हें विस्तृत और संशोधित करना तथा सूक्ष्मतया या प्रत्यक्ष रूप में उनका मूल्य बदल देना। किसी प्राचीन सिद्धान्त की प्राणवंतता उसी हद तक होती है जिस हद तक वह ऐसे परिवर्तन के लिए स्वाभाविक रूप से अपने-आपको अनुकूल बना लेता है; क्योंकि उसका अर्थ यह होता है कि उसके विचार के रूप की सीमाएँ या अव्यवहार्यताएँ जो भी रही हों, फिर भी इसके अंतर्तत्त्व का सत्य, जीवंत दृष्टि एवं अनुभूति का सत्य, जिसके आधार पर इसकी प्रणाली का निर्माण हुआ था, वह अब तक भी अक्षुण्ण है और एक स्थायी सत्यता अथवा प्रामाणिकता तथा सार्थकता रखता है। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो असाधारण रूप से दीर्घ काल से बनी हुई है और यह आज भी प्रायः उतनी ही नूतन है और अपने वास्तविक सार-तत्त्व में अभी भी बिल्कुल उतनी ही नवीन है - क्योंकि इसे अनुभूति में सदा ही पुनः साक्षात् किया जा सकता है जितनी कि यह तब थी जब यह पहले-पहल महाभारत में प्रकाशित हुई थी या उसकी रूपरेखा के अंदर लिखी गयी थी। भारत में अभी भी यह उन महान् शास्त्रों में से एक के रूप में स्वीकार की जाती है जो अत्यंत प्रामाणिक अथवा अधिकारपूर्ण रूप से धार्मिक चिंतन को नियंत्रित करते हैं और इसकी शिक्षा को भी, वह पूर्ण रूप से स्वीकृत न हो तब भी, सभी संप्रदायों द्वारा उसे परम मूल्यवान् माना जाता है। इसका प्रभाव केवल दर्शनसंबंधी या विद्याध्ययन संबंधी अथवा सैद्धांतिक ही नहीं है अपितु प्रत्यक्ष एवं जीवंत है, एक ऐसा प्रभाव जो चिंतन और कर्म दोनों पर हो, और इसके विचार वास्तविक रूप से एक जाति और संस्कृति के पुनरुज्जीवन एवं नव-जागरण में एक प्रबल निर्माणकारी शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में एक महान् वाणी [व्यक्तित्व] द्वारा यह भी कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें जिन किन्हीं भी आध्यात्मिक सत्यों की आवश्यकता है वे सभी गीता में प्राप्त हो सकते हैं। उस उक्ति को अत्यन्त शाब्दिक अर्थ में लेना इस ग्रंथ के विषय में अंध-विश्वास को प्रोत्साहित करना होगा। आत्मा का सत्य अनंत है और उसे इस प्रकार से परिसीमित नहीं किया जा सकता। तथापि यह कहा जा सकता है कि अधिकतर प्रधान सूत्र इसमें विद्यमान हैं और आध्यात्मिक अनुभूति एवं उपलब्धि के समस्त परवर्ती विकास के होते हुए भी हम अब भी एक विशाल अनुप्रेरणा एवं मार्गदर्शन हेतु इसकी ओर मुड़ सकते हैं।
अतः, गीता के इस अध्ययन में हमारा उद्देश्य इसके विचारों की पांडित्यपूर्ण या शास्त्रीय आलोचना अथवा इसके दार्शनिक सिद्धांत को आत्मतत्त्वसंबंधी अनुसंधान के इतिहास के अन्दर ले आना न होगा, न ही हम इसके साथ विश्लेषणात्मक तर्कशास्त्री की रीति से ही व्यवहार करेंगे। हम इसके पास सहायता और प्रकाश पाने के लिये आते हैं और इसमें हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इसमें से इसका वह सारभूत और जीवंत संदेश खोज निकालें, जिसे मनुष्य जाति को अपनी पूर्णता और अपनी उच्चतम आध्यात्मिक भवितव्यता के लिए ग्रहण करना है।
II. उपदेश का सारमर्म
यहाँ एक ऐसी सुस्पष्ट धारणा की विशेष रूप से आवश्यकता है जो गीता के सारभूत विचार, उसकी शिक्षा के केंद्रीय मर्म को पकड़े रहे, क्योंकि अपने समृद्ध और बहुमुखी विचार से संपन्न होने के कारण तथा आध्यात्मिक जीवन के नानाविध पहलुओं का समालिंगन करने तथा प्रतिपादन की धाराप्रवाह घुमावदार गति से युक्त होने के कारण, अन्य सद्ग्रंथों की अपेक्षा अधिक रूप में, गीता अपने-आप को एक पक्षपातपूर्ण बुद्धि से पैदा हुए एकपक्षीय भ्रांत निरूपण के प्रति खोल देती है।.....
इस प्रकार, ऐसे लोग हैं जिनके अनुसार गीता कर्म-योग का प्रतिपादन बिल्कुल भी नहीं करती, अपितु जीवन को और सब कर्मों को संन्यास के लिये तैयार करनेवाली एक साधना का उपदेश करती है: नियत कर्मों को अथवा जो कोई कर्म सामने आ पड़े उसका तटस्थ अथवा उदासीन निष्पादन ही साधन या साधना है; जीवन और सब कर्मों से अंततः संन्यास ही एकमात्र वास्तविक लक्ष्य है। गीता से ही उद्धरण लेकर और गीता की ही चिंतन-पद्धति में यत्र-तत्र विशिष्ट रीति से बल देकर इस मत को प्रमाणित करना सर्वथा सरल हो जाता है, विशेषकर तब जब संन्यास जैसे शब्द के उस विशेष प्रयोग की ओर से हम अपनी आँखें मूँद लेते हैं जिस विशेष अर्थ में गीता इसका प्रयोग करती है। परन्तु ऐसे मत पर और अधिक डटे रहना तब सर्वथा असंभव हो जाता है जब पक्षपातरहित होकर व्यक्ति देखता है कि ग्रंथ में अंत तक बारंबार इसी पर बल दिया गया है कि अकर्म की अपेक्षा कर्म ही श्रेष्ठ है और समत्व के द्वारा कामना का सच्चा और आंतरिक त्याग कर के कर्मों को परमपुरुष को अर्पण करने में ही वरीयता है।
फिर कुछ अन्य लोग इसका वर्णन इस रूप में करते हैं मानो भक्ति-तत्त्व का प्रतिपादन ही गीता की संपूर्ण शिक्षा हो और ऐसा बताकर गीता के अद्वैत तत्त्वों को, और सभी कुछ के एकमेव ब्रह्म में शांत भाव से निवास करने की स्थिति को इसमें जो ऊँचा स्थान दिया गया है उसको पृष्ठभूमि में डाल देते हैं अर्थात् उसकी अवहेलना करते हैं। और निस्संदेह गीता का भक्ति पर दिया बल, इसके द्वारा भगवान् के इस पहलू पर आग्रह कि वे ईश्वर और पुरुष हैं, और फिर इसका पुरुषोत्तम सिद्धान्त जो परम् पुरुष को क्षर और अक्षर पुरुष दोनों से ही श्रेष्ठ सिद्ध करता है और जो कि वही हैं जिन्हें जगत् के सम्बन्ध से हम ईश्वर कहते हैं, ये सब गीता के अत्यंत विलक्षण तथा इसके अत्यंत प्रधान तत्त्वों में से हैं। तो भी, ये ईश्वर ही वह आत्मा हैं, जिनमें संपूर्ण ज्ञान की परिणति होती है, और [ये ही] यज्ञ के प्रभु हैं, सभी कर्म जिनकी ओर ले जाते हैं, और ये ही प्रेममय स्वामी हैं जिनकी सत्ता में भक्तिमय हृदय प्रवेश पाता है। और गीता [इन तीनों में] पूर्ण रूप से उचित संतुलन बनाए रखती है, कहीं ज्ञान पर बल देती है, कहीं कर्म पर और कहीं भक्ति पर, परन्तु वह बल उसके तात्कालिक विचार-प्रसंग के प्रयोजन से होता है, न कि इनमें से किसी एक को दूसरों से पृथक् पूर्ण वरीयता देने के लिए होता है। जिनमें इन तीनों का समागम होता है और मिलकर एक हो जाते हैं, वे ही परम् पुरुष पुरुषोत्तम हैं।
परन्तु वर्तमान में, वस्तुतः जबसे आधुनिक बुद्धि ने गीता को मानना और उस पर थोड़ा-बहुत विचार करना आरम्भ किया है, तब से लोगों की प्रवृत्ति गीता के ज्ञानतत्त्व और भक्तितत्त्व को गौण मानकर, उसके कर्म पर दिये निरंतर आग्रह का फायदा उठाकर उसे एक कर्मयोग-शास्त्र, कर्म-मार्ग में ले जानेवाला प्रकाश, कर्म-विषयक शास्त्र ही मानने की ओर दिखायी देती है। निस्संदेह गीता एक कर्म-योग-शास्त्र है, परंतु उन कर्मों का जिनकी परिसमाप्ति ज्ञान में अर्थात् आध्यात्मिक सिद्धि में और शांति में होती है, उन कर्मों का जो भक्ति-प्रेरित हैं, अर्थात् अपनी समग्र सत्ता का पहले परम् पुरुष के हाथों में और फिर उनकी सत्ता में सचेतन समर्पण, और यह किसी भी प्रकार उन कर्मों का शास्त्र नहीं है जैसा कि आधुनिक मन कर्मों से समझता है, उन कर्मों का बिल्कुल नहीं जो अहंकार और परोपकार के भाव से किये जाते हैं या जो वैयक्तिक, सामाजिक और मानवतावादी प्रयोजनों, सिद्धान्तों और आदर्शों से प्रेरित होते हैं। फिर भी आधुनिक टीकाएँ गीता का यही अभिप्राय दिखाने की चेष्टा करती हैं। कितनी ही प्रामाणिक वाणियों या सत्ताओं द्वारा हमें बारंबार यह बताया जाता है कि भारतीय विचार और आध्यात्मिकता की जो सामान्य तपश्चर्यात्मक और निवृत्तिमार्गी प्रवृत्ति है, उसका खण्डन करते हुए गीता बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मानव कर्म के सिद्धान्त की, सामाजिक कर्तव्यों का निःस्वार्थ भाव से निर्वाह करने के आदर्श की, इतना ही नहीं, अपितु (ऐसा लगता है कि) समाजसेवा के सर्वथा आधुनिक आदर्श की भी घोषणा करती है। इन सब बातों का उत्तर मेरे पास इतना ही है कि गीता में, स्पष्ट ही, और केवल इसका ऊपरी अर्थ ग्रहण करते हुए भी, इस तरह की कोई बात नहीं है, यह केवल आधुनिकों द्वारा गलत अर्थ लगाया जाना है, यह एक प्राचीन ग्रंथ का आधुनिक बुद्धि के अनुसार अर्थ लगाना है, एक सर्वथा पुरातन, सर्वथा प्राच्य और भारतीय शिक्षा को वर्तमान यूरोपीय या यूरोपीय रंग में रंगी बुद्धि के अनुरूप पढ़ने की चेष्टा करना है। गीता जिस कर्म का प्रतिपादन करती है वह कोई मानवीय नहीं अपितु दिव्य कर्म है; कोई सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं अपितु कर्त्तव्य अथवा आचरण के अन्य सभी मानदण्डों को त्याग कर भागवत् संकल्प का निष्काम पालन है जो कि हमारी प्रकृति के द्वारा क्रिया करता है; कोई समाजसेवा नहीं, अपितु सर्वश्रेष्ठ, भगवताविष्टों, महापुरुषों का कर्म है जो निर्वैयक्तिक अथवा अनासक्त भाव से संसार के लिये, तथा उन भगवान् के प्रति यज्ञ-रूप से किया जाता है जो मनुष्य और प्रकृति के पीछे अवस्थित हैं।...
अतः आज की मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से गीता की व्याख्या करना और गीता से सर्वोच्च और सर्वसंपूर्ण धर्म के रूप में हमें निःस्वार्थ कर्तव्यपालन की बलपूर्वक शिक्षा दिलाना, एक त्रुटि है। जिस प्रसंग से गीतोपदेश हुआ है उसका किंचिन्मात्र विचार करने से ही यह स्पष्ट हो जायेगा कि गीता का ऐसा अभिप्राय हो ही नहीं सकता था। क्योंकि, इस उपदेश का संपूर्ण कारण, जिस प्रसंग से इसका आविर्भाव हुआ है और जिस कारण से शिष्य को गुरु की शरण लेनी पड़ी उसका मूल तो कर्तव्य की परस्पर संबद्ध विविध भावनाओं का जटिल रूप से उलझा हुआ वह संघर्ष है जिसका अंत मानव-बुद्धि के द्वारा खड़े किये गए सारे उपयोगी बौद्धिक और नैतिक भवन के ढहने में होता है। मनुष्य-जीवन में किसी-न-किसी प्रकार का संघर्ष प्रायः ही उत्पन्न हुआ करता है, जैसे कभी गार्हस्थ्य-धर्म के और देश-धर्म या किसी उद्देश्य या अभियान की पुकार के बीच दुविधा, कभी स्वदेश के दावे और मानव जाति की भलाई या किसी बृहत्तर धार्मिक या नैतिक सिद्धांत के बीच संघर्ष। यहाँ तक कि एक आन्तरिक संकट या समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसी कि गौतम बुद्ध के जीवन में उपस्थित हुई थी, जिसमें अंतःस्थित भगवान् के आदेश का पालन करने के लिए सभी कर्त्तव्यों को त्याग देना, कुचल डालना और एक ओर फेंक देना होता है। मैं नहीं समझता कि गीता इस प्रकार के आंतरिक संकटकाल का समाधान बुद्ध को पुनः अपनी पत्नी और पिता के पास भेजकर और उन्हें पुनः शाक्य राज्य की बागडोर हाथ में देकर करेगी; न ही यह एक रामकृष्ण को किसी स्वदेशी पाठशाला में पंडित बनकर छोटे बालकों को निष्काम भाव से पाठ पढ़ाने का निर्देश करेगी; न ही यह एक विवेकानन्द को अपने परिवार के भरण-पोषण करने के लिए बाध्य करेगी और इसके लिए वीतराग होकर वकालत या चिकित्सा या पत्रकारिता का पेशा अपनाने को कहेगी। गीता निःस्वार्थ कर्त्तव्य पालन की नहीं अपितु दिव्य जीवन के अनुकरण की शिक्षा देती है, 'सर्वधर्मान्', सभी धर्मों का परित्याग कर के, एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय ग्रहण करने की शिक्षा देती है; और एक बुद्ध, रामकृष्ण या विवेकानन्द का भगवद्-कर्म गीता की इस शिक्षा से पूर्णतः समस्वर अथवा अनुरूप है। यही नहीं, यद्यपि गीता कर्म को अकर्म से श्रेष्ठ मानती है, परंतु कर्म-संन्यास का निषेध नहीं करती, अपितु इसे भी भगवान् तक पहुँचने के अनेक मार्गों में से एक के रूप में स्वीकार करती है। यदि उसकी प्राप्ति केवल कर्म तथा जीवन तथा सभी कर्त्तव्यों के त्याग करने से ही होती हो और भीतर से पुकार प्रबल हो तो इन सबको अग्नि में होम कर ही देना होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं चल सकता। भगवान् की पुकार अलंघ्य है, और अन्य किन्हीं भी हेतुओं के सामने इसकी तुलना नहीं की जा सकती।
इसके सदृश अन्य किसी भी महान् ग्रंथ की तरह ही गीता को इसकी संपूर्णता में पढ़कर तथा एक उत्तरोत्तर विकसनशील विचार के रूप में इसका अध्ययन करने पर ही समझना सम्भव है। परन्तु आधुनिक टीकाकारों ने, बंकिमचंद्र चटर्जी जैसे उच्च कोटि के लेखक से आरंभ कर, जिन्होंने पहले-पहल गीता को, इस नए अर्थ में, कर्त्तव्य निष्पादन का अर्थ प्रदान किया, गीता के पहले तीन या चार अध्यायों पर ही प्रायः पूर्ण बल दिया है, और उनमें भी समता के विचार पर और 'कर्तव्यं कर्म' की उक्ति पर, जिसका अभिप्राय वही है जो आधुनिक दृष्टि में कर्त्तव्य शब्द से समझा जाता है, और इस उक्ति पर बल दिया जाता है कि 'कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर्मफल में जरा भी नहीं' जिसे कि गीता के महावाक्य के रूप में प्रचलित तौर पर उद्धृत किया जाता है। और उच्च दर्शन अथवा तत्त्वज्ञानसंपन्न शेष अठारह अध्यायों को गौण महत्त्व प्रदान किया जाता है, हाँ, अवश्य ही ग्यारहवें अध्याय के विश्वरूप-दर्शन को छोड़कर। आधुनिक बुद्धि के लिए ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक है जो कि तत्त्वसंबंधी सूक्ष्मताओं तथा अतिदूरवर्ती आध्यात्मिक अनुसंधानों के प्रति असहिष्णु होती है या अभी कल तक भी असहिष्णु रही है, और अर्जुन के समान ही कर्म में रत होने को आतुर रहती है तथा मुख्य रूप से कर्म के किसी व्यवहार्य विधान 'धर्म' से ही प्रयोजन रखती है। परंतु गीता जैसे ग्रंथ से व्यवहार करने का यह अनुचित तरीका है।
(ii.47)
xviii 66
प्रश्न : जबकि गीता का महावाक्य है: 'सर्वधर्मान् परित्यज्य....' फिर भी आम तौर पर जब भी गीता की चर्चा होती है तब अधिकांश लोग 'कर्मण्येवाधिकारस्तु...', कि तुम्हारा केवल कर्म का अधिकार है, फल का नहीं, ऐसे ही विचारों पर विशेष बल क्यों देते हैं और जो महावाक्य है उस पर विशेष ध्यान नहीं देते?
उत्तर : स्वयं गीता में तीसरे ही अध्याय में भगवान् कहते हैं कि 'कर्म तो मेरी ही प्रकृति करती है, केवल मूढ़जन ऐसा समझते और कहते हैं कि वे स्वयं कर्मों के कर्ता हैं।' परंतु जिन टीकाकारों को इस बात का कोई गहरा अनुभव नहीं होता वे ही इस प्रकार की उक्ति कर सकते हैं कि गीता कर्म को ही प्रधान बता रही है। और फिर विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा गीता पर लिखी टीकाओं में इस विचार पर बल देने के कारण ही यह आम प्रचलन में इस तरह समझा जाता है। परंतु फल की इच्छा रखे बिना किये जाना वाला यह निष्काम कर्म वास्तव में तो हम जीवन में लागू हो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कामना-रहित कर्म करना क्या हमारे वश में है? इस कर्म की विषमता को देखकर ही तो अर्जुन यह पूछता है कि ऐसा कर्म संभव ही कैसे हो सकता है। यदि कामना न हो तो व्यक्ति कर्म करेगा ही क्यों और यदि करेगा भी तो विभिन्न कर्मों व विकल्पों के बीच उसके लिए चुनाव करने का आधार ही क्या होगा? इसी के उत्तरस्वरूप भगवान् यज्ञरूप से कर्म करने के विचार का निरूपण करते हैं कि 'सारा जीवन यज्ञमय बनाओ, 'मेरी' प्रसन्नता के निमित्त कर्म करो। इसी से तुम्हारी समस्या का हल होगा।' श्रीअरविन्द की गीता के ऊपर टीका से प्रभावित होकर ही योगी श्रीकृष्णप्रेम ने दिलीप कुमार रॉय को कहा था कि हर हिन्दुस्तानी को इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें जिन तत्त्वों का निरूपण हुआ है, वे और कहीं नहीं मिल सकते। इसी से प्रभावित होकर श्री दिलीप कुमार श्रीअरविन्द के संपर्क में आए व उनके शिष्य बने।
प्रश्न : क्या ऐसा कह सकते हैं कि श्रीअरविन्द के पूर्ण योग में सभी योग-पद्धतियों के समन्वय होने के पूर्व गीता ही एक सर्वाधिक समन्वयकारी पुस्तक रही है जो सभी योग-पद्धतियों को लेकर उनका समन्वय साधते हुए उन्हें अतिक्रम कर जाती है?
उत्तर : अवश्य ही, इसीलिए इसे सर्वोच्च ग्रंथ, हिन्दु धर्म की बाइबल के रूप में माना जाता है। ऐसा नहीं था कि श्रीअरविन्द की टीका से पहले किसी को गीता के ऐसे समन्वयात्मक स्वरूप की समझ न हो। परंतु आधुनिक मानसिकता के लिये इसे समझ पाना कठिन है। जिस तरह के कर्म की शिक्षा तथाकथित आधुनिक बुद्धिजीवी गीता के द्वारा दिलवाना चाहते हैं वैसी किसी चीज पर गीता का कोई बल नहीं है। वह तो ईश्वर के निहित कर्म करने की बात करती है। इसमें भगवान् बड़े ही स्पष्ट रूप से अर्जुन को अपनी शरण में आने का निर्देश करते हैं। स्वयं श्रीअरविन्द के योग का आधार भी यह पूर्ण आत्म-समर्पण ही है। इन सब विषयों को श्रीअरविन्द पर्याप्त रूप से प्रकट करेंगे।
गीता कर्मयोग से आरंभ करती है और कर्मयोग के चलते-चलते ज्ञानयोग को समाविष्ट कर लेती है। और फिर उन दोनों के साथ भक्तियोग में प्रवेश कर जाती है। भगवान् के प्रति पूर्ण समर्पण ही योग की इस संपूर्ण गति की परिणति है। पर गीता का महावाक्य तो असंदिग्ध रूप से एक ही है – सर्वधर्मान् परित्यज्य - और स्वयं गीता ही यह बता रही है। इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि गीता का महावाक्य क्या है। जैसे कि श्रीअरविन्द जब स्वयं कहते हैं कि उन्होंने अपने योग में भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है तो यदि कोई कहे कि श्रीअरविन्द के योग में कर्म को ही प्रधानता दी गई है तो यह एक बेतुकी बात होगी। और वास्तव में अपने-आप में ये परस्पर भिन्न चीजें भी नहीं हैं। यदि व्यक्ति के अंदर भक्ति हो तो वह भगवान् के लिए कर्म भी करेगा। यदि कोई कहे कि वह भगवान् का भक्त तो है पर उनके लिए कर्म नहीं करता, तो इसका अर्थ है कि उसकी भक्ति पूर्ण नहीं है। इनके साथ ही साथ उसमें ज्ञान भी आ जाएगा, क्योंकि यदि ज्ञान न हो तो भक्ति अपूर्ण रहती है जिसके बिना सच्चा कर्म भी नहीं हो सकता। इसलिए यदि समग्र भक्ति होगी तो ज्ञान भी अवश्य ही आ जाएगा।
जिस समता का गीता उपदेश करती है वह उदासीनता नहीं है, गीता के उपदेश की आधारशिला रखे जाने और उस पर उपदेश की प्रधान संरचना के निर्मित होने के पश्चात्, अर्जुन को दिये इस महान् आदेश कि, "उठ, शत्रुओं का संहार कर और एक समृद्ध राज्य का भोग कर", में किसी अटल परोपकारवाद की या किसी विशुद्ध विकार-रहित आत्म-त्याग के भाव की ध्वनि तक नहीं है; गीता की समता एक आंतरिक संतुलन और विशालता की स्थिति है, जो कि आध्यात्मिक मुक्ति की आधारशिला है। इस संतुलन से युक्त होकर और इस मुक्तावस्था में हमें उस 'कर्तव्यं कर्म' को करना है, यह एक ऐसी उक्ति है जिसे गीता अत्यंत व्यापकता के साथ प्रयोग करती है जिसमें 'सर्वकर्माणि', सभी कर्मों का समावेश है, और जो भले ही सामाजिक कर्त्तव्यों या नैतिक दायित्वों को अपने अंदर समाविष्ट रखती हो पर उनका अतिशय रूप से अतिक्रम कर जाती है। वह कर्तव्यं कर्म क्या है, इसका निर्धारण व्यक्तिगत पसंद से नहीं होना है; और न कर्म का अधिकार और कर्मफल का त्याग ही गीता का महावाक्य है, अपितु यह एक आरंभिक उपदेश है जो योगपर्वत पर चढ़ना आरम्भ करने वाले शिष्य की प्राथमिक अवस्था पर लागू होता है। इसकी आगामी अवस्था में इस उपदेश का लगभग अधिक्रमण ही कर दिया जाता है। क्योंकि इससे आगे गीता प्रभावपूर्ण रूप से इसकी स्थापना करती है कि मनुष्य कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म की कर्जी तो (दिव्य) प्रकृति है, कर्म के त्रिगुणमय रूपों से संपन्न महान् शक्ति है जो उसके द्वारा कार्य करती है, और मनुष्य को यह देख लेना सीखना होगा कि कर्म का कर्ता वह नहीं है। इसलिए 'कर्मण्येवाधिकारः' का भाव तभी तक लागू होता है जब तक कि हम कर्त्तापन के भ्रम में हैं, और जैसे ही हम स्वयं अपनी चेतना के लिए अपने कर्मों के कर्तापन का भाव त्याग देते हैं वैसे ही कर्मफलाधिकार के समान ही कर्माधिकार भी मन-बुद्धि से निश्चय ही तिरोहित हो जाता है। तब समस्त कर्म-विषयक अहंकार, चाहे वह फलाधिकार का हो या कर्माधिकार का, समाप्त हो जाता है।
परन्तु प्रकृति का नियतिवाद गीता का अंतिम वचन नहीं है। मन, हृदय और बुद्धि के साथ भगवच्चेतना में प्रवेश करने और उसमें निवास करने के लिए बुद्धि की समता और फल का त्याग तो केवल साधनमात्र हैं; और गीता ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि इन्हें साधनस्वरूप तब तक प्रयोग में लाना होगा जब तक कि साधक इस योग्य नहीं हो जाता है कि वह इस भगवच्चेतना में रह सके या कम-से-कम अभ्यास के द्वारा इस उच्चतर अवस्था को स्वयं में क्रमशः विकसित करने का प्रयास न कर ले। और यह भगवान् क्या है जो कि श्रीकृष्ण स्वयं होने की घोषणा करते हैं? ये पुरुषोत्तम हैं, जो अकर्ता पुरुष के परे हैं, जो कर्नी प्रकृति के परे हैं, जो एक के आधार हैं और दूसरे के स्वामी, ये वे प्रभु हैं जिनका यह सारा प्राकट्य है, जो हमारी वर्तमान मायावशता की अवस्था में भी प्रकृति के नियमों का नियमन करते हुए अपने जीवों के हृदय में विराजमान हैं, ये वे हैं जिनके द्वारा कुरुक्षेत्र की समरभूमि की सेनाएँ जीवित होती हुई भी पहले ही मारी जा चुकी हैं और जो अर्जुन को इस भीषण संहारकर्म का केवल यंत्र या निमित्त मात्र बनाए हुए हैं। प्रकृति उनकी केवल कार्यकारिणी शक्ति है। साधक को इस प्रकृति-शक्ति और उसके त्रिविध गुणों से ऊपर उठना होगा, उसे त्रिगुणातीत होना होगा। उसे अपने कर्म प्रकृति को नहीं समर्पित करने होंगे, जिन पर कि अब उसका कुछ भी दावा या 'अधिकार' नहीं है, अपितु उन परम् पुरुष की सत्ता में समर्पित करने होंगे। अपना मन, बुद्धि, हृदय, तथा संकल्प उन्हीं में आश्रित कर, आत्म-ज्ञान के साथ, भगवद्-ज्ञान के साथ, जगत्-संबंधी ज्ञान के साथ, पूर्ण समता, अनन्य भक्ति और पूर्ण आत्म-दान के साथ उसे अपने कर्म उन प्रभु की भेंट-स्वरूप करने होंगे जो सारे तपों और समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। उनके संकल्प के साथ एकसंकल्प और उनकी चेतना से सचेतन होना होगा और वे 'तत्' पुरुष ही कर्म का निर्णय और प्रारंभ करेंगे। यही वह समाधान है जो भगवान् गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं।
गीता का महान्, परम वचन, इसका महावाक्य क्या है हमें उसे ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं; क्योंकि स्वयं गीता ही अपने अंतिम श्लोकों में उस महान् संगीत का परम स्वर घोषित करती है। "अपने हद्देशस्थित भगवान् की, सर्वभाव से, शरण ले, उन्हीं के प्रसाद से तू पराशांति और शाश्वत पद को लाभ करेगा। मैंने तुझे गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान बताया है। अब उस गुह्यतम ज्ञान को, उस परम वचन को सुन जो मैं अब बतलाता हूँ। मेरे मन वाला (मन्मना) हो जा, मेरा भक्त बन, मेरे प्रति यज्ञ कर, और मेरी अर्चना कर; तू निश्चय ही मेरे पास आयेगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय जो है। सभी धर्मों का परित्याग कर के केवल मेरी शरण ग्रहण कर। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा; शोक मत कर।"
गीता का प्रतिपादन अपने-आपको तीन महान् सोपानों में बाँट लेता है, जिनके द्वारा कर्म मानव-स्तर से ऊपर उठकर दिव्य स्तर तक पहुँच जाता है और वह उच्चतर धर्म की मुक्तावस्था के लिए निम्नतर धर्म-बंधनों को नीचे ही छोड़ जाता है। पहले सोपान में, मनुष्य द्वारा कामना का त्याग कर, पूर्ण समता के साथ कर्ताभाव से यज्ञ-स्वरूप कर्म किया जाता है, यह यज्ञ उन ईश्वर के लिए किया जाता है जो परम हैं और एकमात्र आत्मा हैं, यद्यपि अभी तक इनको व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी सत्ता में अनुभव नहीं किया गया है। यह आरंभिक सोपान है। दूसरा सोपान है केवल फलेच्छा का ही त्याग नहीं, अपितु कर्मों के कर्तापन के भाव का भी त्याग इस अनुभूति में करना होता है कि आत्मा सम, अकर्ता, अक्षर तत्त्व है और सब कर्म विश्व-शक्ति के, परं प्रकृति के हैं जो विषम, कर्ती और क्षर शक्ति है। अंतिम सोपान में, परम् आत्मा को ऐसे परम-पुरुष के रूप में जान लेना होगा जो प्रकृति के नियामक हैं, जिनके कि प्रकृतिगत जीव आंशिक अभिव्यक्ति हैं, और जिनके द्वारा अपनी पूर्ण परात्पर स्थिति में रहते हुए प्रकृति के द्वारा सारे कर्म कराए जाते हैं। उन्हें ही प्रेम, आराधना और कर्मों का यजन अर्पित करना होगा; सारी सत्ता उन्हीं को समर्पित करनी होगी और संपूर्ण चेतना को ऊपर उठाकर इस भागवत् चेतना में निवास करना होगा जिससे कि जीव भगवान् की प्रकृति और कर्मों से परे उनकी दिव्य परात्परता में भागी हो सके और पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति की अवस्था में रहते हुए कर्म कर सके।
प्रथम सोपान है कर्मयोग, (भगवत्प्रीत्यर्थ) निष्काम कर्मों का यज्ञ; और यहाँ गीता का आग्रह कर्म पर है। द्वितीय है ज्ञानयोग, आत्मा और जगत् के सत्स्वरूप का ज्ञान तथा आत्म-उपलब्धि; यहाँ आग्रह ज्ञान पर है; पर साथ-साथ निष्काम कर्म भी चलता रहता है, यहाँ कर्ममार्ग ज्ञानमार्ग के साथ एक हो जाता है पर उसमें घुल-मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खो देता। तृतीय अथवा अंतिम सोपान है भक्तियोग, परमात्मा की भगवान् अथवा दिव्य पुरुष के रूप में उपासना और खोज; यहाँ आग्रह भक्ति पर है; पर ज्ञान को गौण नहीं बनाया गया है, अपितु वह उन्नत हो जाता है, अनुप्राणित अथवा सशक्त हो जाता है और परिपूर्ण हो जाता है, और कर्मों का यज्ञ अब भी जारी रहता है; द्विविध मार्ग अब ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिविध मार्ग बन जाता है। और, यज्ञ का फल, एकमात्र फल जो साधक के सामने ध्येयरूप से अभी तक रखा हुआ है, प्राप्त हो जाता है, अर्थात् भगवान् के साथ ऐक्य और परम् दिव्य प्रकृति के साथ एकत्व साधित हो जाता है।
पहला अध्याय
कुरुक्षेत्र
संसार के अन्य महान् धर्मग्रंथों के बीच गीता की विलक्षणता यह है कि वह अपने-आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में स्थित नहीं है; न यह बुद्ध, ईसा या मुहम्मद जैसे किसी मौलिक अथवा सृजनशील व्यक्तित्व के आध्यात्मिक जीवन का या फिर वेदों और उपनिषदों के समान किसी विशुद्ध आध्यात्मिक अनुसंधान के युग का ही फल है, अपितु यह राष्ट्रों और उनके संग्रामों तथा मनुष्यों तथा उनके पराक्रमों के ऐतिहासिक महाकाव्य के अन्दर एक उपाख्यान है जिसका प्रसंग इसके एक प्रमुख पात्र के जीवन में उपस्थित एक विकट संकट-काल से पैदा हुआ है जिसमें कि उस पात्र के समक्ष उसके जीवन का ऐसा कर्म उपस्थित है जिसमें अन्य कर्मों की परिपूर्णता होने वाली है; एक ऐसा कर्म जो भयंकर, अति प्रचंड और रक्तपातपूर्ण है, और एक ऐसा क्षण या ऐसी निर्णायक घड़ी उपस्थित है जब उसे या तो इस कर्म से विल्कुल परावर्तन करना होगा या इसे (इन सब रक्तपातों में से होते हुए) इसकी निर्दय पूर्णाहुति तक पहुँचाना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता - जैसा कि आधुनिक समालोचकों का मानना है कि ऐसा ही है कि गीता महाभारत के बाद की रचना है या नहीं, जिसे इसके रचयिता ने इसे महाभारत में इसलिए मिला दिया कि इसकी शिक्षा को भी इस महान् राष्ट्रीय महाकाव्य की प्रामाणिकता और लोकप्रियता का लाभ मिल जाए। मुझे लगता है कि इस धारणा के विपक्ष में बड़े प्रबल प्रमाण हैं और इस पक्ष में भीतरी बाहरी जो कुछ प्रमाण हैं वे अत्यंत अपर्याप्त और स्वल्प हैं। परन्तु यदि यह मत सही अथवा यथेष्ट भी हो तो भी यह तथ्य तो शेष रहता है कि ग्रंथकार ने न केवल अपने इस ग्रंथ को महाभारत की बुनावट में इस प्रकार जटिलता से बुनकर घुला-मिला देने का अथक श्रम किया है कि इसके ताने-बाने को महाभारत से अलग नहीं किया जा सकता, अपितु वह हमें बार-बार वह प्रसंग भी याद दिलाने में सावधान है जिस प्रसंग से यह गीतोपदेश किया गयाः और यह प्रसंग की ओर लौटने का कार्य वह प्रकट रूप से केवल उपसंहार के समय ही नहीं करता, अपितु अपने गंभीरतम तत्त्वनिरूपण के बीच में भी करता है। हमें ग्रंथकार का यह आग्रह मानना ही होगा और इस गुरु-शिष्य-संवाद में गुरु और शिष्य दोनों का ही यह जिस प्रसंग की ओर बारंबार ध्यान खींचता है उसे उसका पूर्ण महत्त्व प्रदान करना ही होगा। इसलिए अवश्य ही गीता के सिद्धान्त को मात्र किसी सामान्य अध्यात्मदर्शन या नीतिशास्त्र के रूप में न देखकर नीतिशास्त्र और अध्यात्मशास्त्र को मानव जीवन पर प्रत्यक्षतः प्रयुक्त करने पर व्यवहार में जो संकट उपस्थित होता है उसे दृष्टिगत रखते हुए इस ग्रंथ पर विचार करना होगा।
धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १॥
१. धृतराष्ट्र ने कहाः हे सञ्जय । धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया?'
सञ्जय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ।।२।।
२. सञ्जय ने कहाः पांडवों की सेना को व्यूह रचना में खड़ी देखकर राजा दुर्योधन ने अपने आचार्य (द्रोणाचार्य) के समीप जाकर ये वचन कहे :
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ।।३।।
३. हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की गयी पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिये।
-----------------------
'गीता की व्याख्या की एक ऐसी पद्धति भी है जिससे न केवल यह उपाख्यान ही अपितु संपूर्ण महाभारत ही मनुष्य के आंतरिक जीवन का एक रूपकमात्र बन जाता है, और फिर उसका हमारे इस बाह्य मानवीय जीवन तथा कर्म से कोई संबंध नहीं रहता, अपितु इसका संबंध केवल अंतरात्मा और हमारे अन्दर अधिकार जमाने के लिये लड़नेवालो शक्तियों के बीच युद्ध से रह जाता है। यह एक ऐसा मत है जिसकी पुष्टि इस महाकाव्य के सामान्य स्वरूप और इसकी वास्तविक भाषा से नहीं होती, और यदि इस विचार पर बहुत अधिक जोर दिया जाए, तो गीता को सीधी-सादी दार्शनिक भाषा आदि से अंत तक क्लिष्ट, कुछ-कुछ निरर्थक दुर्बोधता में बदल जाएगी। वेद की और कम-से-कम पुराणों के कुछ अंश की भाषा स्पष्ट रूप से रूपकात्मक है, जो कि अलंकारों और स्थूल दृष्यमान जगत् के आवरण के पीछे रहनेवाली वस्तुओं के मूर्त प्रतिरूपों के वर्णन से भरी पड़ी है, परंतु गोता तो विल्कुल स्पष्ट शब्दावली में लिखी गई है और मनुष्य के जीवन में जो बड़ी-बड़ी नैतिक और आध्यात्मिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं उन्हीं को हल करने का दावा करती है, अतः यह अनुचित होगा कि इस स्पष्ट भाषा और सुस्पष्ट विचारों के पीछे जाकर और अपनी कल्पनाओं को संतुष्ट करने हेतु मन के अनुसार तोड़-मरोड़कर उनका अर्थ लगाया जाए।
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्व महारथः ।।४।।
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ।।५।।
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्व वीर्यवान् ।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ।।६।।
४-६. इस विशाल सेना में महाधनुर्धारी शूरवीर हैं जो लड़ने में भीम और अर्जुन के समान हैं; जैसे युयुधान (सात्यकि) और विराट और महारथी राजा द्रुपद। धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान् काशिराज, पुरुजित्, और कुन्तिभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य और पराक्रमी युधामन्यु और बलवान् उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र (अभिमन्यु) और द्रौपदी के (पाँचों) पुत्र; ये सब ही महारथी हैं।
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ।।७।।
७. हे द्विजश्रेष्ठ! अब हमारे पक्ष में जो विशिष्टगण हैं, मेरी सेना के नायक हैं, आपकी जानकारी के लिये उनके नाम कहता हूँ, उन्हें जान लीजिये।
भवान्भीष्मश्च कर्णश्व कृपश्च समितिञ्जयः ।
अश्वत्थामा विकर्णश्व सौमदत्तिस्तथैव च ॥८॥
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।
नानाशखप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ।।९।।
८-९. आप तथा (पितामह) भीष्म और कर्ण, संग्रामविजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा और विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा; इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिये जीवन का उत्सर्ग कर दिया है, अनेक प्रकार के शखाखों से सुसज्जित, ये सभी युद्ध करने में निपुण हैं।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ।।१०।।
१०. भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी यह सेना अपरिमित है। किंतु भीम के द्वारा रक्षित इनकी यह सेना परिमित (परिमाण और बल में कम) है।
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ।।११।।
११. इसलिये युद्ध के सब प्रवेश-द्वारों पर अपने-अपने यथा निर्धारित स्थानों (मोचौं) पर खड़े रहकर आप सब के सब ही भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें।
तस्य सञ्जनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः ।
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्ख दध्मौ प्रतापवान् ।।१२।।
१२. तब महाप्रतापी कुरुवंश के वृद्ध भीष्मपितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करते हुए ऊँचे स्वर से सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शङ्ख बजाया।
ततः शङ्खाश्व भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ।।१३।।
१३. तदनंतर शङ्ख और नगारे और ढोल, मृदंग और रणशृङ्गी सहसा ही बज उठे, उनका वह शब्द महाप्रचंड हुआ।
ततः श्वेतैहयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शड्डौ प्रदध्मतुः ।।१४।।
१४. इसके अनंतर श्वेत घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठे हुए श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अर्जुन ने भी अपने-अपने दिव्य शङ्खों को बजाया।
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
पौण्डूं दध्मौ महाशङ्ख भीमकर्मा वृकोदरः ।।१५।।
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्व सुघोषमणिपुष्पकौ ।।१६।।
१५-१६. हृषीकेश (श्रीकृष्ण) ने पाञ्जजन्य नामक शङ्ख को, धनञ्जय (अर्जुन) ने देवदत्त नामक शङ्ख को और भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर (भीमसेन) ने पौण्ड्र नामक महाशङ्ख को बजाया । कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंतविजय नामक शङ्ख को तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शङ्खों को बजाया।
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्वापराजितः ।।१७।।
द्रुपदो द्रौपदेयाश्व सर्वशः पृथिवीपते ।
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक् ।।१८।।
१७-१८. हे राजन् ! महा-धनुर्धारी काशिराज और महारथी शिखण्डी, धृष्टद्युम्न और विराट और अजेय सात्यकि, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सुभद्रातनय अभिमन्यु इन सबने चारों ओर से पृथक् पृथक् अपने शङ्खों को बजाया।
स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ।।१९।।
१९. उस महाप्रचंड शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया।
अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः ।
प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।।२०।।
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।
२०-२१. हे राजन् ! इसके अनंतर कपिध्वज वाले पांडुपुत्र अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित रूप में खड़े देखकर शस्त्र प्रहार के प्रारंभ होने का समय आने पर उस समय अपने धनुष को उठाकर हृषीकेश (श्रीकृष्ण) से ये वचन कहे।
अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । ॥२१॥
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् ।
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ।।२२।।
२१-२२. अर्जुन ने कहाः हे अच्युत! (अनघ, अचल श्रीकृष्ण !) मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थित करो, जिससे कि मैं युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन विपक्षियों का निरीक्षण कर लूँ और यह जान सकूँ कि इस रणरूपी महोत्सव में मुझे किन-किन के साथ युद्ध करना है।
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ।।२३।।
२३. धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा से जो यहाँ आये हुए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देख लूँ।
कोरे फलमूलक अथवा व्यावहारिक मनुष्य की यह विशेषता है कि वह अपने संवेदनों के द्वारा ही अपने कर्म के आशय के प्रति सचेत होता है। अर्जुन ने अपने सखा और सारथी से अपने को दोनों सेनाओं के बीच में अवस्थित करने को कहा, किसी गंभीर विचार से नहीं, अपितु उन असंख्यों मनुष्यों का मुँह एक निगाह में देख लेने की उस दंभयुक्त मंशा से जो अधर्म का पक्ष लेकर आये हैं और जिनका अर्जुन को इस रण रूपी महोत्सव में सामना करना है, जिन्हें उसे धर्म की विजय के लिये जीतना और मारना है।
सञ्जय उवाच
एवमुक्तो इषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ।।२४ ।।
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति ॥२५॥
२४-२५. सञ्जय ने कहाः हे घृतराष्ट्र ! गुडाकेश (निद्राविजयी अर्जुन) द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इषीकेश (इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण) ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा कर के ऐसा कहा कि "हे पार्थ! इन एकत्रित हुए कौरवों को देख।"
तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ।
आचार्यान्मातुलान्ध्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥२६॥
श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।
२६-२७. तब अर्जुन ने वहाँ दोनों ही सेनाओं में उपस्थित पिता के सदृशों (चाचाओं-ताऊओं) को, पितामहों, आचायाँ, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और संगी-साथियों को, श्वसुरों को और स्नेहियों को देखा।
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् ।।२७।।
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।
२७-२८. उन सब अपने संबंधियों को इस प्रकार युद्ध के लिये तैयार खड़े देखकर कुन्तीपुत्र अर्जुन अतिशय विषाद से अभिभूत हो, विषाद और संताप से ग्रस्त हो इस प्रकार बोलाः
जैसे ही वह उस दृश्य को देखता है वैसे ही इस गृह-युद्ध और वंश-युद्ध का अर्थ उसकी समझ में आ जाता है- एक ऐसा युद्ध जिसमें न केवल एक ही जाति, एक ही राष्ट्र, एक ही वंश के, अपितु एक ही कुल और एक हो परिवार के लोग एक-दूसरे के विरुद्ध आमने-सामने खड़े हैं। वे सब जिन्हें सामाजिक मनुष्य परम प्रिय और पूज्य मानता है उन्हीं लोगों का उसे शत्रु के नाते सामना करना और वध करना होगा- पूज्यपाद गुरु और आचार्य, पुराने संगी-साथी, मित्र, सहयोद्धा, दादा, चाचा, और वे लोग जो रिश्ते में पिता के समान, पुत्र के समान, पौत्र के समान हैं, वे लोग जिनके साथ रक्त का संबंध है या जो साले-संबंधी हैं, इन सभी सामाजिक बंधनों को तलवार के द्वारा काटना होगा।
यहाँ श्रीअरविन्द अर्जुन की प्रकृति को जिस रूप में प्रकट कर रहे हैं वैसा वर्णन हमें कदाचित ही अन्य किसी टीका में मिलता है। ऐसा नहीं था कि अर्जुन यह नहीं जानता था कि कौन-कौन उनके पक्ष में हैं और कौन-कौन उनके विपक्ष में हैं। इस विषय में वह पूर्णतः अभिज्ञ था। अतः श्रीअरविन्द उसकी प्रकृति को सामने लाकर बता रहे हैं कि अर्जुन एक संवेदन-प्रधान व्यक्ति था न कि विचार-प्रधान। उसकी बुद्धि में संवेदनों के द्वारा ही प्रकाश आ सकता था। इसीलिए जब युद्ध के मैदान में वह पूरा दृश्य उसके सामने आया, वे लोग उसके सामने आए तब उसे यह अनुभव हुआ कि इस युद्ध का वास्तव में अर्थ क्या है। गीता के विचार के निरूपण का क्रम एक ऐसे व्यक्ति के अनुसार है जो व्यावहारिक स्वभाव वाला है, जिसके विचार और धर्म बड़े सुनिर्धारित हैं और सूक्ष्म चीजों में जिसका अधिक प्रवेश नहीं है। इसी कारण अर्जुन को बार-बार प्रश्न पूछने पड़ते हैं। तो ऐसा है अर्जुन का स्वभाव। श्रीअरविन्द ने 'गुरु और शिष्य' शीर्षक से पूरा अध्याय ही इस विषय पर लिखा है।
अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ।।२८।।
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेपथुश्व शरीरे मे रोमहर्षश्व जायते ।।२९।।
२८-२९. अर्जुन ने कहा : हे कृष्ण ! अपने इन स्वजनों को यहाँ युद्ध के लिये समुपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि इन बातों का अर्जुन को पहले पता नहीं था, पर उसको उन सबका जीवंत अनुभव नहीं हुआ था; उसे तो धुन सवार थी अपने अधिकार के दावों की, अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बदले की, अपने जीवन के सिद्धांतों और सही के लिये लड़ने की, न्याय और धर्म की रक्षा कर के तथा अधर्म और अत्याचार से युद्ध कर के उनको मार भगाकर क्षत्रिय-धर्म का पालन करने की। इन सब की धुन में उसने युद्ध के इस पहलू के बारे में न तो कभी गहराई के साथ सोचा न अपने हृदय के अंदर और जीवन के मर्मस्थल में अनुभव ही किया। और अब दिव्य सारथी यह उसकी दृष्टि के सामने लाते हैं, उसकी आँखों के आगे सनसनीखेज तरीके से उपस्थित करते हैं और इससे उसकी संवेदनात्मक, प्राणमय और भावमय सत्ता के मर्म-स्थल पर एक गहरा आघात-सा लगता है।
गाण्डीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।॥३०॥
३०. गाण्डीव (अर्जुन का धनुष) मेरे हाथ से गिरा जा रहा है और त्वचा मानो जली जा रही है। और मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हो रहा हूँ और मेरा मन मानो चक्कर खा रहा है।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।।३१॥
३१. और हे केशव । मुझे विपरीत लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने आत्मीय जनों को मारने में मुझे कोई कल्याण भी नहीं दिखाई देता।
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।।३२।।
३२. हे कृष्ण ! (ऐसी) विजय को मैं नहीं चाहता और न राज्य को चाहता हूँ, न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविन्द ! बतलाओ हमें राज्य से क्या लाभ है, भोगों से क्या लाभ है अथवा जीवन धारण करने से भी क्या प्रयोजन है?
पहला परिणाम होता है एक भाव-संवेदनात्मक और शारीरिक संकटावस्था जो उपस्थित कर्म और उसके भौतिक फलों से और फिर स्वयं जीवन के प्रति ही जुगुप्सा का भाव पैदा कर देती है। वह उस प्राणिक उद्देश्य - सुख और भोग - से अपना मुँह फेर लेता है जिसके अहंभावयुक्त मानव जाति पीछे पड़ी रहती है; वह क्षत्रियों के उस प्राणिक उद्देश्य - विजय, राज्य, अधिकार और मनुष्यों पर शासन करने की (प्रबल लालसा) - से भी अपना मुँह मोड़ लेता है। यदि इसे इसके व्यावहारिक अर्थ में विचारा जाए तो यह धर्मयुद्ध आखिर है किसलिए, सिवाय स्वयं अपने, अपने भाइयों और अपने दलवालों के स्वार्थ अथवा हेतु सिद्ध करने के लिए, अधिकार करने, भोग करने और राज्य करने के लिए? परंतु इतनी बड़ी कीमत पर तो ये प्राप्त करने योग्य ही नहीं हैं, व्यर्थ हैं। इन चीजों का स्वयं अपने में कोई मूल्य भी नहीं है, ये तो केवल सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को सुसंपन्न बनाये रखने के साधनमात्र हैं और अपने परिवार और जाति (race) के लोगों का संहार कर के ठीक इन्हीं उद्देश्यों को ही उसे अभी नष्ट करना होगा। और तब भावनाएँ पुकार उठती हैं।
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।। ३३ ।।
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४॥
३३-३४. जिनके लिये हमें राज्य, भोग और सुख की आकांक्षा हो सकती है, वे ये आचार्यगण, पिता वर्ग (ताऊ-चाचा आदि), पुत्रगण, तथा पितामह, मामा, श्वसुर लोग, पोते, साले, और भी दूसरे संबंधी लोग अपने प्राण और धनों (की आशा) का त्याग कर के युद्ध में उपस्थित हैं।
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ।।३५।।
३५. हे मधुसूदन! (श्रीकृष्ण) भले इनके द्वारा मेरा वध हो जाए पर मैं त्रिलोकी के राज्य के लिये भी इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता, पृथ्वी के आधिपत्य की तो बात ही क्या है?
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ।।३६।।
३६. हे जनार्दन । (श्रीकृष्ण) इन धृतराष्ट्र के पुत्रों (कौरवों) को मारने पर हमें कौन-सा सुख मिल सकता है? यद्यपि ये आततायी हैं तथापि इन्हें मारने पर हम पाप के ही भागी होंगे।
यह सारा प्रकरण ही भयंकर पाप है- क्योंकि अब संवेदनों और भावावेगों के विद्रोह का समर्थन करने के लिये नैतिक बोध जाग उठता है। यह एक पाप है, आपस के लोगों की मार-काट में न कोई धर्मसम्मतता है, न न्यायोचितताः विशेषतः जब कि मारे जानेवाले स्वभावतः ही पूजा और प्रेम के भाजन हैं, जिनके बिना व्यक्ति जीना ही नहीं चाहेगा, और इन पवित्र भावनाओं को भंग करने में कोई पुण्यकर्म नहीं हो सकता, और यह और कुछ नहीं बस घोर पाप हो सकता है।
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् ।
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।। ३७ ।।
३७. अतः हमारे लिये अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों (कौरवों) को मारना उचित नहीं है। क्योंकि हे माधव! हमारे अपने जनों की हत्या कर के हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं?
श्रीअरविन्द इसका सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं कि विषम परिस्थिति उपस्थित होने पर मनुष्य की प्रकृति किस प्रकार प्रतिक्रिया करने लगती है। सबसे पहले तो मन उचट जाता है, भावनाओं को चोट पहुँचती है। युद्ध का एक व्यावहारिक संकट है, और उससे संकुचन को उचित-अनुचित ठहराने के लिए नैतिकता, पाप-पुण्य का बोध आगे आता है। इस तरह व्यक्ति का स्वभाव किसी भी चीज को उचित-अनुचित ठहरा सकता है। इसका मुख्य कारण है कि अर्जुन की प्रकृति इन भावावेगों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है और इससे अपना मुँह मोड़ लेना चाहती है। इसके लिए उसका सारा नैतिक बोध, मन, बुद्धि, धर्म-अधर्म संबंधी उसकी धारणाएँ उसके समर्थन में उतर आते हैं। हम स्वयं भी सारे दिन इसी प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रिया करते रहते हैं। वास्तव में तो, हमारी शारीरिक और प्राणिक प्रकृति को जो अनुकूल नहीं लगता उसे मन नैतिकता से, पुराण-कथाओं आदि के माध्यम से उचित ठहराने का प्रयास करता है, और हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम धोखा खा रहे हैं। गीता इसी से आरंभ करती है कि जिन भावावेगों को अर्जुन सहन नहीं कर पाता है, और उनसे अपने पलायन के समर्थन में जो-जो दलीलें देता है, वे सब किस प्रकार अनुचित और अपर्याप्त हैं। अर्जुन सरीखा भौतिक संवेदनों से चालित व्यक्ति नहीं जानता कि इस तरह की विकट समस्या को कैसे हल करे। वह नहीं जानता कि इसे नैतिक आधार पर, व्यावहारिक आधार पर, या उसे ज्ञात अन्य किसी भी आधार पर उसे कैसे हल किया जा सकता है। इसीलिए वह कहता है कि, "चाहे मेरा सब कुछ नष्ट क्यों न हो जाए, तो भी मुझे ये सब रक्तरंजित सुख-भोग नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसके लिए लडूं ही क्यों?" अर्जुन की इन बातों का मानसिक स्तर पर कोई उत्तर हो भी नहीं सकता। इस तरह की परिस्थिति उसके सामने लायी गयी है और इसके समाधान के तौर पर सबसे पहले उसे उसके क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार कर्तव्यों की तथा अन्य दायित्वों की याद दिलाई गई है जिन्हें अर्जुन स्वीकार करने वाला नहीं है।
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ।।३८ ।।
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ।।३९।।
३८-३९. यद्यपि लोभ के द्वारा इनकी बुद्धि के भ्रष्ट (आच्छादित) हो जाने के कारण ये लोग कुल के क्षय होने से उत्पन्न होनेवाले दोष को और मित्र का अनिष्ट करने में होनेवाले पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन! हम लोग तो कुल के क्षय होने से उत्पन्न होनेवाले दोष को देखते हैं (समझते हैं) तब फिर इस पापकर्म से हटने के लिए हमें अपना विवेक क्यों न काम में लेना चाहिए?
गीता की शिक्षा में हम देखते हैं कि अहंभाव से मुक्ति की जो माँग की जाती है वह कितनी सूक्ष्म वस्तु है। अर्जुन शक्ति के अहंकार एवं क्षत्रिय के अहंकार द्वारा लड़ने के लिये प्रवृत्त होता है; इससे विपरीत उसकी दुर्बलता के अहंकार द्वारा, उसके संकुचन द्वारा, अरुचि के भाव द्वारा तथा मन, स्नायविक सत्ता और इन्द्रियों को अभिभूत करनेवाली मिथ्या 'करुणा' द्वारा उसे युद्ध से पराङ्गमुख कर दिया जाता है, यह वह 'दिव्य करुणा' नहीं जो भुजाओं को सुदृढ़ बनाती है तथा ज्ञान को सुस्पष्ट बना देती है। परन्तु उसकी यह दुर्बलता त्याग का तथा पुण्य का बाना पहनकर आती है: "इन रुधिरलिप्त भोगों को भोगने से तो भिक्षुक का जीवन व्यतीत करना कहीं अच्छा है; मुझे समस्त पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिये, न देवताओं का ही राज्य चाहिए।" हम कह सकते हैं कि गुरु की कितनी बड़ी मूर्खता है कि उसकी इस वृत्ति का समर्थन नहीं किया, संन्यासियों की सेना में एक और महान् आत्मा की वृद्धि करने तथा संसार के सामने पावन त्याग का एक और उज्ज्वल दृष्टान्त उपस्थित करने का यह भव्य अवसर खो दिया। परन्तु दिव्य पथप्रदर्शक, ऐसे पथप्रदर्शक जिन्हें शब्द-आडंबर द्वारा छला नहीं जा सकता, इसे किसी और ही रूप में देखते हैं, "ये दुर्बलता, विभ्रम-मति और अहंकार है जो तेरे अन्दर बोल रहे हैं। आत्मतत्त्व को देख, अपनी आँखें ज्ञान की ओर खोल, अपनी अहंबद्ध आत्मा को शुद्ध कर।" और, उसके बाद? "युद्ध कर, विजय प्राप्त कर, एक समृद्ध राज्य का उपभोग कर।" अथवा प्राचीन भारतीय परंपरा से एक अन्य दृष्टान्त लें। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह अहंकार ही था जिसने अवतारी पुरुष राम को लंका के राजा से अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करने के लिये एक सेना खड़ी करने तथा एक राष्ट्र का विनाश करने को उद्यत किया। परन्तु क्या यह इससे कम अहंकार होता यदि वे उदासीनता का जामा पहन ज्ञान के प्रचलित शब्दों का दुरुपयोग करते हुए कहते, "मेरी कोई पत्नी नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई कामना नहीं; ये तो इन्द्रियों के भ्रम हैं, मुझे तो ब्रहा-ज्ञान का संवर्द्धन करना चाहिये और जनक की पुत्री के साथ रावण जो चाहे करे।"
जैसा कि गीता बलपूर्वक कहती है, इसकी कसौटी भीतर है। वह यह कि अन्तरात्मा को लालसा और आसक्ति से मुक्त रखा जाये, परंतु साथ ही इसे अकर्म के प्रति आसक्ति से तथा कर्म करने के अहंपूर्ण आवेग से भी मुक्त रखा जाए, पुण्य के बाह्य रूपों के प्रति आसक्ति तथा पाप के प्रति आकर्षण - दोनों से ही एक समान मुक्त रखा जाये। एकमेव आत्मतत्त्व में निवास करने तथा उस एकमेव आत्मतत्त्व में कर्म करने के लिये 'मैं-पन' और 'मेरा-पन' से मुक्त होना होगा; विराट् (वैश्विक) पुरुष के किसी व्यक्ति-विशिष्ट केन्द्र के द्वारा कर्म करने से इंकार करने के अहंकार का त्याग करना और साथ ही सब कुछ को छोड़कर केवल अपने वैयक्तिक मन, प्राण और शरीर की सेवा करने के अहंकार का भी त्याग करना होगा। आत्मा में निवास करने का अर्थ यह नहीं कि निर्व्यक्तिक आत्मानन्द के उस महासागर में निमग्न हो सब वस्तुओं से बेखबर एकमात्र अपने हित उस अनन्त के अंदर निवास किया जाए; अपितु इसका अर्थ है उस (परम) आत्मा की तरह और उस आत्मा में निवास करना जो इस देह में तथा सब देहों में और साथ ही सब देहों से परे भी समान रूप से विद्यमान है। यही पूर्णज्ञान है।
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो ऽभिभवत्युत ।॥४०॥
४०. कुल का क्षय होने से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाता है; और धर्म के नष्ट हो जाने पर अधर्म संपूर्ण कुल को अभिभूत कर लेता है।
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।
खीषु दुष्टासु वाष्र्णेय जायते वर्णसङ्करः ।।४१।।
४१. हे कृष्ण ! अधर्म की अभिवृद्धि हो जाने से कुल की स्त्रियाँ दुश्चरित्र हो जाती हैं। है वार्णेय (श्रीकृष्ण) । स्त्रियों के दुश्चरित्र होने पर वणाँ का सांकर्य उत्पन्न होता है।
सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।।४२।।
४२. वर्णसांकर्य कुलनाशक लोगों को और स्वयं कुल को भी नरक में ले जाने का कारण बनता है; क्योंकि पिण्ड और जल की क्रिया के लुप्त हो जाने से इनके पितर (पितृलोक से) गिर जाते हैं।
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः ।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्व शाश्वताः ।।४३।।
४३. कुलघातियों के इन वर्णसांकर्य के उत्पादक दोषों से सनातन जातिधर्म और कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं।
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ।।४४।।
४४. हे जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो गये हैं उन मनुष्यों का नरक में निश्चय ही निवास होता है। ऐसा हमने सुना है।
अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ।।४५।।
४५. अहो ! खेद की बात है कि हम लोगों ने बहुत बड़े पाप (के) करने का निश्चय किया है जो हम राज्यसुख के लोभ से अपने आत्मीय जनों का वध करने के लिये तैयार हुए हैं।
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शत्रपाणयः ।
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ।।४६।।
४६. इसकी अपेक्षा यदि शस्त्रों से रहित और कुछ भी प्रतिकार न करते हुए मुझको शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डालें तो यह मेरे लिये अधिक कल्याणकारी होगा।
सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः । ॥४७॥
४७. सञ्जय ने कहाः युद्धभूमि में ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्यथित-चित्त हो गया और बाणसहित धनुष को परित्याग कर के रथ के पिछले भाग में अपने स्थान पर बैठ गया।
.....यद्यपि अर्जुन को केवल अपनी ही परिस्थिति से, अपने ही आंतरिक संघर्ष और कर्म-विधान से मतलब है, तथापि जैसा कि हम देख चुके हैं, जो विशेष प्रश्न अर्जुन ने उठाया है और जिस ढंग से उठाया है वह वास्तव में मनुष्य-जीवन और कर्म के सारे ही प्रश्न को सामने ले आता है। यह संसार क्या है और क्यों है और जैसा यह है उसमें इस सांसारिक जीवन का आत्मजीवन के साथ कैसे मेल बैठे? इस समस्त गहरे और कठिन विषय का दिव्य गुरु ठीक उस आधारशिला के स्थापन के रूप में हल करना चाहते हैं जिस पर वे उस कर्म का आदेश देते हैं जिसे सत्ता के एक नवीन सन्तुलन से और एक मोक्षप्रद ज्ञान के प्रकाश द्वारा करना होगा।
तब फिर वह कौन-सी चीज है जो उस मनुष्य के लिए कठिनाई उपस्थित करती है जिसे इस संसार को, जैसा यह है, वैसा ही स्वीकार करना है और इसमें कर्म करना है और साथ ही अपने अन्दर की सत्ता में, आध्यात्मिक जीवन में निवास करना है। संसार का यह पहलू क्या है जो उसके जागृत मन को व्याकुल कर देता है और ऐसी अवस्था ला देता है जिसके कारण गीता के प्रथम अध्याय का नाम 'अर्जुन-विषादयोग' सार्थक हुआ; वह विषाद और निरुत्साह जो मानव-जीव को तब अनुभूत होता है जब यह संसार जैसा है ठीक वैसा ही, अपने असली रूप में उसके सामने आता है और उसे इसका सामना करना पड़ता है, जब आचार और नेकी के भ्रम का परदा आँखों के सामने से, और किसी बड़ी चीज के साथ उसका मेल होने से पहले ही, फट जाता है? यह वह पहलू है जिसने बाह्य रूप से कुरुक्षेत्र के नर-संहार और रक्तपात के रूप में आकार ग्रहण किया है और आध्यात्मिक रूप से समस्त वस्तुओं के स्वामी के कालरूप-दर्शन के रूप में जो उन प्राणियों का भक्षण करने और नष्ट करने के लिये प्रकट हुए हैं जिन्हें स्वयं उन्होंने रचा है।.... जीवन एक युद्ध और एक संहारक्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है; ये भगवान् महाभयंकर हैं, यही दर्शन अर्जुन को उस समर भूमि पर दृष्टिगोचर होता है।
....यदि हम जरा भी भगवान् की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जैसा कि गीता स्वीकार करती है, कहने का तात्पर्य है कि यदि वे ऐसे सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् हैं फिर भी सदा परात्पर-पुरुष हैं जो जगत् को प्रकट कर के स्वयं भी उसमें प्रकट होते हैं, जो अपनी माया, प्रकृति या शक्ति के दास नहीं, अपितु प्रभु हैं, जो अपनी जगत्-संकल्पना या रूपरेखा में अपने ही बनाए जीव-जन्तुओं, मानव-दानव द्वारा बाधित या कुंठित नहीं किये जा सकते, जिन्हें अपनी सृष्टि या अभिव्यक्ति के किसी भाग के उत्तरदायित्व को अपने सृष्ट या अभिव्यक्त प्राणियों के ऊपर लादकर स्वयं उससे मुक्त होने अथवा अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है; (यदि हम ऐसा स्वीकार करते हैं) तब तो मानव को एक महान् और दुःसाध्य श्रद्धा धारण कर के ही आगे बढ़ना होगा। जब मानव अपने-आपको एक ऐसे जगत् में पाता है जो देखने में युद्धरत शक्तियों की एक भीषण विश्रृंखलता, विशाल और अंधकारमय शक्तियों का संग्राम प्रतीत होता है, जहाँ जीवन सतत् परिवर्तन और मृत्यु द्वारा ही टिका हुआ है, और जो व्यथा, यंत्रणा, अमंगल और विनाश की विभीषिका द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है, और जब ऐसे जगत् के अन्दर उसे सभी में सर्वव्यापी ईश्वर को देखना होता है और इस बात के प्रति सचेतन होना होता है कि इस पहेली का कोई हल अवश्य है और यह कि जिस अज्ञान में वह अभी निवास करता है उसके परे कोई ऐसा ज्ञान है जो इन विरोधों में सामंजस्य स्थापित कर देता है, तो उसे इस श्रद्धा के आधार पर खड़ा होना होगा कि, 'भले तुम मुझे मार भी डालो, फिर भी मैं तुम्हारा भरोसा ही करूंगा।' समस्त मानव चिंतन अथवा श्रद्धा जो सक्रिय और निश्चयात्मक होती है, चाहे वह ईश्वरवादी हो, सर्वेश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी हो, वह निश्चित तौर पर न्यूनाधिक स्पष्टता और पूर्णता के साथ इस प्रकार के किसी भाव को अपने में रखती है। यह स्वीकार करती है और विश्वास करती है : स्वीकार करती है जगत् को विसंगतियों को, और विश्वास करती है भगवान्, वैश्विक सत्ता या 'प्रकृति' के किसी उच्चतम तत्त्व में जो हमें इन विसंगतियों को अतिक्रम करने, अतिक्रांत या विजित करने तथा समस्वर करने में समर्थ बनाएगा, और कदाचित् ये तीनों ही क्रियाएँ एक साथ करने में समर्थ बनाएगा कि अतिक्रम और अतिक्रांत करने के द्वारा समस्वरता चरितार्थ करें।
यहाँ उपस्थित प्रश्न एक बड़ा ही मूलभूत प्रश्न है। सारी मनुष्यजाति के लिए सदा से ही यह बड़ी विकट समस्या रही है। श्रीअरविन्द कहते हैं कि यद्यपि अन्य कुछ ने इसका अपने तरीके से समाधान करने का प्रयास किया है परंतु हिन्दुस्तान ने ही मूलभूत रूप से इसका हल किया है। गीता उसी प्रश्न को सामने ला रही है, यही कुरुक्षेत्र है, कि हमारे समाज में सब जगह एक प्रचलित धारणा यह है कि परमात्मा, अल्लाह, गॉड – भले हम जिस भी नाम से उन्हें पुकारें - बड़े ही दयालु हैं। और वेदान्त तो यहाँ तक कहता है कि वे स्वयं ही इन सब रूपों को धारण किए हुए हैं। इसलिए यह तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वे स्वयं के साथ कोई अनुचित व्यवहार करेंगे। उनकी प्रवृत्ति स्वयं को पीड़ित करने में आनंद लेने की या फिर दूसरों को सताने में आनंद लेने की नहीं है। कोई भी धर्म इस पर विश्वास नहीं करता। अब यदि हम चीटियों के दृष्टिकोण से इस संसार को देखें तो उन्हें कदाचित् ही यह रास आता होगा? उसी प्रकार जब हम कमजोरों पर अत्याचार, प्रकृति का दोहन, आपसी लड़ाई-झगड़ा, स्त्रियों पर अत्याचार, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या, बुरे लोगों को शासन आदि करते देखते हैं तो हमारा नैतिक बोध, सौंदर्यात्मक बोध आहत होता है और तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं? जब धर्म का काम है मानव को भगवान् की ओर अभिमुख करना, तो इस समस्या का समाधान करना उसके लिये पहली आवश्यकता बन जाती है।
इस समस्या के समाधान हेतु भिन्न तर्क दिये जाते हैं। एक कहता है कि परमात्मा की बात न मानकर मनुष्य ने त्रुटि की और उसका दण्ड तो उसे भोगना ही पड़ेगा। दूसरा कहता है कि व्यक्ति ने पूर्वजन्म में कोई पाप किये हैं इसलिए उन कर्मों का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। वहीं तीसरा कहता है कि परमात्मा तो दयालु हैं परंतु एक शैतान भी है जो ये सब काम करवाता है। यदि व्यक्ति परमात्मा के विधान के अनुसार चलेगा तो वह शैतान से बच जाएगा अन्यथा शैतान के हाथों में जा गिरेगा और फिर अनेक तरीकों से यंत्रणाएँ पाएगा। इसलिए ये सारे बुरे काम शैतान के कराए हुए हैं। जगत् की विषमताओं के स्पष्टीकरण लिए इस प्रकार के भिन्न-भिन्न तर्क दिये जाते हैं।
परन्तु श्रीअरविन्द यहाँ अपनी टीका में कह रहे हैं कि जो परमात्मा स्वयं ही सभी जगह अभिव्यक्त हो रहे हैं, उन्हें इस सबके लिए मनुष्यों को या उन शक्तियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें उन्होंने स्वयं ही रचा है। वे कमजोर नहीं हैं कि अन्य कोई शक्ति आकर उन्हें सीमित कर सके या उनकी इच्छा को विफल कर सके। भारतीय संस्कृति के अंदर इस विषय में सदा ही स्पष्ट बोध रहा है कि परमात्मा की इच्छा ही एकमात्र प्रभावी होती है। तब फिर कुरुक्षेत्र का जैसा भयंकर स्वरूप है और जिस प्रकार का परम दयालु स्वरूप परमात्मा का बताया जाता है, इन दोनों में मेल कैसे बैठाया जाए? बाह्य प्रतीतियों के स्तर पर इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। इसलिये जो ईश्वर की सत्ता को मानने वाला है, सद्भाव वाला, सहृदय व्यक्ति है उसे तो इस सुदृढ़ श्रद्धा का आश्रय लेना ही पड़ेगा कि भले ही प्रतीति में बुराई शासन करती है, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या होती है, और यद्यपि वह स्वयं भी इससे ग्रस्त है और स्वयं तकलीफ में आ सकता है तो भी परमात्मा तो सदा कल्याण ही करते हैं।
अतः इसके समाधान हेतु दूसरा तर्क दिया जाता है कि जिस प्रकार माता-पिता अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं परन्तु कई बार बच्चों को उनका किया हुआ समझ न आने के कारण बहुत बुरा लगता है उसी प्रकार परमात्मा तो हमारे भले के लिए ही सब कुछ करते हैं किन्तु हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं और जिस दिन हमारे अन्दर चेतना जागृत होगी उस दिन हम इसका अर्थ समझ जाएँगे, और जब हम समझ जाएँगे तो भगवान् के सहयोग से इससे ऊपर उठ जाएँगे और ऐसी भव्यताओं में प्रवेश करेंगे जो कि परमात्मा हमारे लिए संजोए हुए हैं पर जिनकी हम अब कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सकारात्मक आध्यात्मिकता है। इसमें व्यक्ति देखेगा कि परमात्मा केवल करालवदना काली ही नहीं हैं, वे उदार माता भी हैं। अतः अर्जुन को हल तब मिलेगा जब वह इस कुरुक्षेत्र को एक कम भयाक्रांत दृष्टि से देखेगा, जो कि मानव दृष्टि की एक मूलभूत समस्या है।
प्रश्न : तो फिर कर्म-विधान और संस्कार का आधार क्या है?
उत्तर : यह तो केवल एक स्पष्टीकरण है, एक व्याख्या करने का तरीका मात्र है। अन्यथा इस सब प्रपंच की, घोर प्रतीतियों की व्याख्या कैसे की जाए। क्योंकि हमारे नैतिक बोध के अनुसार यदि कोई अच्छे काम करे और उसके साथ भी बुरा बर्ताव हो या बुरे परिणाम आएँ, तो इसकी व्याख्या कैसे की जाए। अतः या तो इसके लिए भगवान् पर दोष मँढ़ा जाए या फिर पिछले जन्मों में किये कर्म-विधान का तरीका निकाला जाए।
[क्योंकि] भगवान् केवल संहारकर्ता ही नहीं अपितु सब प्राणियों के परम सुहृद् भी हैं; केवल वैश्विक त्रिदेव ही नहीं अपितु परात्पर पुरुष भी हैं; जो करालवदना काली हैं वे स्नेहमयी मंगलकारिणी माता भी हैं; कुरुक्षेत्र के प्रभु दिव्य सखा और सारथी भी हैं, सब प्राणियों के मनमोहन हैं, साक्षात् (अवतारी) श्रीकृष्ण हैं। और इस संग्राम, संघर्ष और विश्रृंखला में से होकर वे हमें जहाँ कहीं भी ले जा रहे हों, जिस भी लक्ष्य या देवत्व तक वे हमें आकृष्ट कर रहे हों, परंतु इसमें संदेह नहीं कि वे हमें इन सभी पहलुओं की किसी परात्परता तक ले जा रहे हैं...पर कहाँ, कैसे, किस प्रकार की परात्परता से, किन परिस्थितियों से, यह हमें ढूँढ़ना होगा, और इसे ढूँढ़ने के लिये पहली आवश्यकता है कि इस जगत् को जैसा यह है वैसा देखें, और उनकी क्रिया आरम्भ में और अब जैसे-जैसे अपने-आप को प्रकट करती जाए वैसे-वैसे उसका अवलोकन करते जाएँ और उसका उचित मूल्यांकन करते जाएँ, इसके बाद उनका मार्ग और लक्ष्य बेहतर रूप में स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएँगे। इससे पूर्व कि हम अमर जीवन की ओर हमारे मार्ग को खोज सकें, हमें कुरुक्षेत्र को स्वीकार करना होगा, हमें मृत्यु के द्वारा जीवन का जो विधान है उसे स्वीकार करना होगा। हमें अवश्य ही अपनी आँखें खोलकर, अर्जुन की अपेक्षा कम व्यथित दृष्टि से, काल और मृत्यु के हमारे स्वामी का दर्शन करना होगा और इस वैश्विक संहारकर्ता* को अस्वीकार करने, इससे घृणा करने या इससे भयभीत होने की वृत्ति को छोड़ देना होगा।....केवल कुछ ही ऐसे धर्म रहे हैं जिन्होंने भारत के सनातन धर्म के समान निःसंकोच रूप से यह कहने का साहस किया है कि यह रहस्यमय विश्व-शक्ति एक भगवत्तत्त्व है, एक त्रिमूर्ति है; जिसने कि इस जगत् में क्रियारत शक्ति के स्वरूप को न केवल परोपकारी दुर्गा के रूप में ही ऊँचा नहीं उठाया अपितु रक्तरंजित संहार-नृत्य करनेवाली, करालवदना काली के रूप में भी प्रतिष्ठित करने और यह कहने का साहस किया है कि "यह भी परम माता है; इन्हें भी परमेश्वरी जानो और यदि तुममें सामर्थ्य हो तो इनका भी पूजन करो।" यह बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है कि जिस धर्म में ऐसी अचल सत्यनिष्ठा और ऐसा प्रचण्ड साहस रहा था वही ऐसी गंभीर और व्यापक आध्यात्मिकता का निर्माण करने में सफल हो सका, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि सत्य ही वास्तविक आध्यात्मिकता का आधार है और साहस उसकी आत्मा।
जो चर्चा हम पहले कर चुके हैं यह उसी का विस्तार है। परमात्मा के रचनात्मक और विनाशकारी दोनों ही रूपों को स्वीकार करना होगा। कुरुक्षेत्र को इस दृष्टि से देखना होगा कि इसके पीछे भी प्रभु की लीला है, जिसे हम भले ही समझ तो नहीं सकते परन्तु फिर भी जिसके पीछे कुछ-न-कुछ शुभ अवश्य है। हिन्दुस्तान ने कभी ऐसा नहीं माना कि भगवान् कुछ गलत करते हैं या उनका कोई विरोधी है जो ऐसा करता है, या फिर उनका विनाशकारी पक्ष तो बहुत खराब है और सृजनात्मक पक्ष बहुत अच्छा है। उन्होंने तो काली को भी माता माना है। और जिसमें यह साहस नहीं है कि इस दृश्य का सामना कर सके उसके लिए वास्तव में आध्यात्मिकता का कोई मूल्य नहीं है। अब अर्जुन के लिए आवश्यक है कि कुरुक्षेत्र को जिस आक्रोश से, जिस भाव से वह देखता है उसकी बजाय अधिक गहरे दृष्टिकोण से देखे, इस श्रद्धा के साथ देखे कि इस सब के पीछे कोई शुभ छिपा है। इसी स्थिति तक ले जाने के लिए और उसे समझाने के लिए कि इसका क्या अर्थ है श्रीकृष्ण, जब अर्जुन ने वह रूप देखने की इच्छा प्रकट की तब, ग्यारहवें अध्याय में उसे वह दिखाते हैं और फिर सारी चीजें समझाते हैं।
अभी यह गीता का आरम्भ है कि वास्तव में जगत् जैसा दृश्यमान होता है उसमें किस तरह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण या भाव रखा जा सकता है, और उसे रखते हुए व्यावहारिक जीवन में क्रिया की जा सकती है। इस प्रश्न का हल यही है कि इस सबको हमें इस श्रद्धा के साथ देखना होगा कि इसके पीछे भगवान् का कल्याणकारी हाथ है भले हम इसे समझ न पाते हों। इसे समझने के लिए हमें उस चेतना में जाना होगा जहाँ हम इसे समझ सकते हैं कि जहाँ भगवान् का रूप भयंकर महाकाली का है, तो वहीं महालक्ष्मी का भी है, श्रीकृष्ण का रूप जहाँ विनाशक कालपुरुष का है, तो वहीं सखा, प्रिय, मधुर बोलने वाले का भी है और साथ ही चार हाथों वाले विष्णु का अभयदान देने वाला रूप भी है और जहाँ इन सबका समन्वय हो सकता है।
यहाँ हमें स्मरण रखना होगा कि गीता की रचना ऐसे समय में हुई थी जब युद्ध मानव क्रियाकलाप का आज से भी अधिक आवश्यक अंग था और जीवन की व्यवस्था से उसके बहिष्कार का विचार तब एक पूर्ण रूप से असंभाव्य अथवा काल्पनिक बात होती। विश्व-शांति और मनुष्यों में पूर्ण सद्भाव का सिद्धांत - क्योंकि बिना एक विश्वव्यापी और पूर्ण पारस्परिक सद्भाव के कोई सच्ची और स्थायी शान्ति नहीं हो सकती हमारी क्रमोन्नति
----------------
* मानव की दृष्टि को भले शुभ लगे अथवा अशुभ, केवल शुभ के लिए ही गुप्त संकल्प कार्य कर सकता है। हमारी नियति दोहरे अर्थों में लिखित हैः 'प्रकृति' के द्वंद्वों द्वारा हम भगवान् के सन्निकट पहुँचते हैं, अंधकार से निकले हैं पर फिर भी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु तो अमरता की ओर हमारा पथ है।
'त्राहि-त्राहि' जगत् की अभिशप्त वाणियाँ पुकारती हैं, फिर भी अंततः शाश्वत 'शिव' विजयी होता है।
के इतिहास में एक क्षण के लिये भी मानवजीवन को अधिकृत करने में सफल नहीं हुआ है, क्योंकि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से जाति इसके लिए तैयार नहीं थी और अपने विकासक्रम में प्रकृति का संतुलन या उसकी स्थिति ऐसे किसी भी अतिक्रमण हेतु अपने को आकस्मिक रूप से तैयार करने की स्वीकृति नहीं देती। अभी तक भी हम लोगों ने वास्तव में किसी ऐसी व्यवस्था की संभावना से परे विकास नहीं किया है जहाँ परस्पर विरोधी स्वार्थों के बीच यथासंभव कोई समझौता कर लेने की प्रवृत्ति न हो, जिससे कि घोर-संघर्षों की पुनरावृत्ति को कुछ कम किया जा सके।.... संभवतः एक दिन आ सकता है, हम तो कहेंगे, निश्चय ही आयेगा, जब मनुष्य-जाति आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक रूप से सर्वव्यापी शांति के राज्य के लिए तैयार होगी; किंतु तब तक किसी भी व्यावहारिक तत्त्वज्ञान और धर्म को, युद्ध के पहलू को और मनुष्य के योद्धा-रूप स्वभाव और कर्तव्य को स्वीकार कर उसका समाधान करना ही होगा। जीवन को अपने वर्तमान स्वरूप में ही लेते हुए, न कि केवल इस रूप में कि किसी सुदूर भविष्य में उसका स्वरूप क्या होगा, गीता यह प्रश्न करती है कि जीवन के इस पहलू तथा क्रिया को, जो कि वास्तव में मनुष्य की सर्वसाधारण गतिविधि का ही अंग और स्वभाव है, किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन के साथ सुसमंजस किया जा सकता है।
मानव की न्यायनिष्ठता के लिए यह उसका वैश्विक अपराध है,
उस सर्वशक्तिमान् का शुभ और अशुभ से परे रहना
पुण्यात्मा को इस दुष्ट जगत् में उनके भाग्य के भरोसे छोड़
इस भयंकर दृश्य में पापात्मा को राज करने देना।
सब कुछ प्रतीत होता है विरोध और संघर्ष और संयोग,
एक निरुद्देश्य श्रम और बहुत अल्प अर्थ,
उन आँखों के लिए जो एक अंश देखती हैं, और समग्र को चूक जाती हैं...
इस प्रकार पहला अध्याय 'अर्जुनविषादयोग' समाप्त होता है।
दूसरा अध्याय
I. आर्य-क्षत्रिय का धर्ममत
सञ्जय उवाच
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ।।१।।
१. सञ्जय ने कहाः इस प्रकार विषाद से भरे हुए, आँसुओं से भरपूर और व्याकुल नेत्रोंवाले, निरुत्साह और शोक से अभिभूत हृदय वाले अर्जुन से मधुसूदन (श्रीकृष्ण) ने ये वचन कहेः
अर्जुन की प्रथम आवेशपूर्ण अहंपरक शंकाओं की बाढ़ के लिए, संहार कर्म से पीछे हटने, उसके दुःख और पाप के बोध, एक रिक्त और निःसार जीवन के लिए शोक-संताप और पाप कर्म से होने वाले पापमय परिणामों के पूर्वानुमान के लिए, दिव्य गुरु का उत्तर है एक कड़े शब्दों में फटकार।
श्रीभगवान् उवाच
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।
अनार्यजुष्टमस्वर्ण्यमकीर्तिकरमर्जुन ।।२।।
२. श्रीभगवान् ने कहाः हे अर्जुन। इस कठिनाई एवं संकट की घड़ी में यह विषाद (कश्मल) तेरे में कहाँ से आ गया है? यह आर्य (श्रेष्ठ) जनों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता; न यह स्वर्ग की प्राप्ति कराता है और न ही कीर्ति की।
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।।३।।
३. हे पार्थ! नपुंसकता को मत प्राप्त हो; यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप! (शत्रुओं का दमन करने वाले) अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का परित्याग कर के (युद्ध के लिये) खड़ा हो।
क्या हम कहेंगे कि यह तो एक वीर का दूसरे वीर को वीरोचित उत्तर है, किन्तु वह नहीं जिसकी हम दिव्य गुरु से आशा करते हैं; इसके विपरीत उनसे क्या यह आशा नहीं की जानी चाहिये कि वे सदा मृदुता, साधुता एवं आत्मत्याग के भावों को तथा सांसारिक ध्येयों से पीछे हटने और संसार की रीतियों से छूट निकलने को ही प्रोत्साहित करेंगे? गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि अर्जुन अवीरोचित दुर्वलता में जा पड़ा है... क्योंकि वह करुणा से आक्रांत, 'कृपयाविष्टम्', हो गया है। तो क्या यह दैवी दुर्बलता नहीं है? क्या करुणा एक दिव्य भावावेग नहीं है, जिसे इस प्रकार की कड़ी फटकार के साथ निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? अथवा क्या हम किसी ऐसी शिक्षा के समक्ष तो नहीं हैं जो केवल युद्ध और वीर कर्म का ही उपदेश देती हो...स्वयं परम गुरु ही आगे के एक अध्याय में दैवी सम्पदा के गुणों को गिनाते हुए प्राणीमात्र पर दया, मृदुता, क्रोध से तथा हिंसा और कष्ट देने की कामना से मुक्ति आदि को निर्भयता, ओज और तेज के बराबर ही आवश्यक बतलाते हैं। क्रूरता, कठोरता, भयानकता और शत्रुओं के वध में हर्ष, धन-संचय और अन्यायपूर्ण भोग आसुरी सम्पदाएँ हैं, इनकी उत्पत्ति उस प्रचण्ड आसुरी प्रकृति से होती है जो जगत् में और मनुष्य में भगवान् की सत्ता को अस्वीकार करती है और केवल कामना को ही अपना आराध्यदेव जानकर पूजती है। तो फिर ऐसे किसी दृष्टिकोण से तो अर्जुन की दुर्बलता फटकारी जाने योग्य नहीं है...
एक दैवी करुणा है जो हमारे पास ऊपर से उतरती है...यह करुणा युद्ध और संघर्ष को, मनुष्य के बल और उसकी दुर्बलता को, उसके पुण्यों और पापों को, उसके हर्ष और संताप को, उसके ज्ञान और अज्ञान को, उसकी बुद्धिमत्ता और मूर्खता को, उसकी अभीप्सा और उसकी असफलता (आदि द्वंद्वों) को एक प्रेम, ज्ञान और शांत स्थिर सामर्थ्य की दृष्टि से देखती है और उनमें प्रवेश कर के सबकी सहायता करती और सबके क्लेश का निवारण करती है। साधु और परोपकारी में यह अपने-आप को प्रेम या उदारता की बहुलता के रूप में मूर्तिमान कर सकती है; विचारक और वीर में यह उपकारी प्रज्ञा एवं बल की विशालता तथा शक्ति का रूप धारण करती है। यही आर्य योद्धा की वह करुणा, उसके शौर्य का प्राण है जो किसी घायल अथवा क्षत-विक्षत को नहीं मारा करती, अपितु दुर्बल की, दलित की, आहत और पतित की सहायता और रक्षा करती है। परन्तु वह भी दिव्य करुणा ही है जो बलिष्ठ आततायी और घृष्ट अत्याचारी को मार गिराती है, किसी प्रकार की घृणा तथा प्रचंड क्रोध के कारण नहीं, क्योंकि ये कोई उच्च दिव्य गुण नहीं हैं, पापियों पर ईश्वर का कोप, दुष्टों से ईश्वर की घृणा इत्यादि बातें अर्द्ध-प्रबुद्ध संप्रदायों की वैसी ही कल्पित कहानियाँ हैं जैसे कि उनके द्वारा आविष्कृत नरकों की अनंत काल तक चलती यातनाओं की कथाएँ – अपितु, जैसा कि प्राचीन आध्यात्मिकता ने स्पष्ट रूप से देखा, कि जब वह बल के मद से मत्त पापी दैत्य का संहार करती है तो ऐसा वह उतनी ही प्रेम और अनुकंपा के साथ करती है जितनी प्रेम और अनुकंपा वह उन दीन-दुखियों और पीड़ितों पर करती है जिन्हें उस दैत्य की हिंसावृत्ति और अन्याय से इसे बचाना होता है।
परन्तु जो अर्जुन को उसके कर्म और लक्ष्य अथवा अभियान का परित्याग करने के लिये उकसा रही है वह कोई इस प्रकार की करुणा नहीं है। वह करुणा नहीं अपितु दुर्बल आत्मदया से परिपूर्ण नपुंसकता है, उस मानसिक यंत्रणा से पीछे हटना या ठिठकना है जो उसके कर्म के फलस्वरूप उसे भोगनी पड़ेगी... और अन्य सभी मनोदशाओं में यह आत्मदया अत्यंत अधम और अनार्य मनोदशाओं में से है। इसका जो दूसरों के प्रति दया का भाव है वह भी आत्म-तुष्टि का ही एक रूप है, यह स्नायुओं का संहारकर्म से भौतिक संकुचन या कातरता है, धार्तराष्ट्रों के विनाश से हृदय का अहंपरक भावावेगमय संकुचन है, क्योंकि 'ये हमारे स्वजन हैं' और इनके बिना तो जीवन ही शून्य हो जाएगा। यह दया मन और इन्द्रियों की एक दुर्बलता है, - ऐसी दुर्बलता उन लोगों के लिये हितकर हो सकती है जो अभी अपने विकासक्रम के निचले स्तर पर हैं, जिन्हें दुर्बल होना ही चाहिये अन्यथा वे क्रूर और कठोर बन जाएँगे; उन्हें अपने कठोरतर रूपों को अपने संवेदनात्मक अहंकार के मृदुतर रूपों के द्वारा सुधारना होगा, उन्हें उस अशक्त तत्त्व, तमोगुण का आवाहन करना पड़ेगा जिससे कि उनके राजसिक आवेशों की उग्रता और अतियों का दमन करने में उस प्रकाशमय तत्त्व, सत्त्वगुण, की सहायता की जा सके। परंतु यह मार्ग उस उन्नत आर्य पुरुष का नहीं है जिसे दुर्बलता के द्वारा नहीं, अपितु शक्ति से और अधिक शक्ति के द्वारा आरोहण करना है। अर्जुन देवमानव है, नरश्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया में है और इसलिए वह देवताओं द्वारा चुना गया है। उसे एक कार्य सौंपा गया है, उसके पास उसके रथ पर स्वयं भगवान् विराजमान हैं, उसके हाथों में दिव्य गांडीव धनुष है और अधर्म के महारथी, संसार में भगवान् के नेतृत्व के विरोधी उसके सामने खड़े हैं। यह निर्णय करने का उसे अधिकार नहीं है कि अपने भावावेगों और आवेशों के अनुसार क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, या अपने अहंपरायण हृदय और बुद्धि की बात मानकर एक आवश्यक विनाश से हट जाए, अथवा इस कारण अपने कर्म से विरत हो जाए कि यह उसके जीवन में दुःख और रिक्तता ला देगा या चूँकि जिन हजारों-हजार (प्राणियों) को अवश्य इसमें नष्ट होना है उनके वियोग की तुलना में इस (कृत्य) के लौकिक परिणाम का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। यह सब उसका अपने उच्चतर स्वभाव से दुर्बलतावश अधःपतन है। उसे तो केवल अपने 'कर्तव्यं कर्म' को देखना होगा, केवल भगवान् के उस आदेश को सुनना होगा जो उसके क्षात्र स्वभाव में से होकर दिया जा रहा है, उसे केवल जगत् और मानव जाति की भवितव्यता के लिए महसूस करना होगा जो उसे अपना देव-प्रेषित मनुष्य जानकर पुकार रहे हैं कि वह जगत् और मानव जाति के प्रयाण में सहायक हो और उसे आक्रांत करने वाली अंधकार की सेनाओं को मारकर उसके पथ को निष्कंटक करे।
यहाँ ध्यान देने की बात यह है, हालाँकि उसका सीधा संबंध इस संदर्भ से तो नहीं है पर वह है महत्त्वपूर्ण, कि मनुष्य की बुद्धि के तर्क बहुत ही सतही प्रकार के होते हैं। हमारी बुद्धि अर्जुन के पक्ष में बड़े अच्छे-अच्छे तर्क दे सकती है क्योंकि हमारे नैतिक दृष्टिकोण, हमारी पसंद के अनुसार हम देखते हैं कि लड़ाई-झगड़े से तो सामंजस्य बेहतर है, पर ऐसे दृष्टिकोणों से देखने पर मनुष्य के निर्णय सौ में से निन्यानवे बार गलत ही होंगे। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी सोच, धारणाओं, दृष्टिकोणों आदि का जैसा स्वरूप है वे अपने-आप में विश्वास के योग्य नहीं हैं। अगर ऐसा न होता तब तो हम आध्यात्मिकता में सहज ही आगे चल पड़ते और हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता ही न होती। परंतु ये चीजें हमें धोखा देती हैं और इनमें से किसी भी चीज का कोईविश्वास नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति को श्रीमाताजी का गहरा स्पर्श प्राप्त नहीं है तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। अन्यथा तो वह केवल अपनी ही चीजों और विचारों को उचित ठहराता रहेगा और इधर-उधर भटकता रहेगा। परंतु ये सभी विषय सतही नहीं हैं, अपितु भीतर से अनुभव करने के हैं। इसका कोई मूल्य नहीं कि हमारे सिद्धांत, हमारे नैतिक मूल्य, हमारे तौर-तरीके क्या हैं, ये सब हमारे कर्म को सच्चे रूप में उचित-अनुचित नहीं ठहरा सकते और कर्म का निर्देशन नहीं कर सकते। कर्म का निर्देशन तो इससे होना चाहिये कि श्रीमाताजी की (भगवान् की) इच्छा क्या है। और गीता के वर्तमान संदर्भ में भी यही बात है। साधना पथ में हम जितना अधिक इस बात को समझ लें कि हमारी अन्तःप्रज्ञा की तुलना में बुद्धि और उसके विचार बड़े ही अपूर्ण, अपर्याप्त तथा निष्प्रभावी हैं, और जितना ही हम इन पर आग्रह रखना बंद कर दें, उतना ही हमारे लिए बेहतर है और मार्ग सुरक्षित हो जाता है। जब तक जीवन में गहरी दृष्टि न हो तब तक कुछ भी सार्थक नहीं किया जा सकता। अन्यथा हम जिस स्थिति में रहते हैं, उसे ही उचित ठहराने वाले तर्क देते रहते हैं और इससे कभी भी हम मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए, यदि हमारे अंदर सच्चा विवेक नहीं है तो हमें कम-से-कम उनका अनुसरण करना चाहिये जिनमें यह है, अन्यथा इस मार्ग में हमारी कोई भी गति नहीं है।
अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ।।४।।
४. अर्जुन ने कहाः हे मधुसूदन (श्रीकृष्ण) ! मैं किस प्रकार युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध (शत्रों) बाणों से युद्ध करूँगा? हे अरिसूदन (शत्रुनाशक)! वे दोनों ही परम पूजनीय हैं।
गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान् ।। ५।।
५. क्योंकि इन महानुभाव गुरुजनों की हत्या की अपेक्षा इस लोक में भिक्षा माँगकर पेट भरना भी श्रेयस्कर है। क्योंकि इन गुरुजनों की हत्या करने पर भी मैं इस लोक में रक्त से सने हुए धन और दूसरे कमनीय पदार्थ-रूप भोगों को ही तो भोगूँगा।
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः।
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।। ६।।
६. और हम यह भी नहीं जानते कि इन दोनों में से कौन-सा हमारे लिये श्रेष्ठ है, कि हम उन पर जय प्राप्त करें अथवा वे हम पर विजयी हों;- हमारे सामने धृतराष्ट्र के पुत्र (पक्ष के लोग) खड़े हैं जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे।
यह उस मनुष्य का संवेदनात्मक, भावावेगात्मक तथा नैतिक विद्रोह है जो अब तक कर्म और उसके प्रचलित मानदंड से संतुष्ट रहा है; पर जो अपने-आप को इन मानदंड और इन कर्मों द्वारा ऐसे भीषण विप्लव में झोंका गया पाता है जहाँ वे एक-दूसरे से और स्वयं के साथ भी भीषण संघर्ष में रत हैं, और खड़े होने के लिए नैतिक आचार-व्यवहार का कोई आधार ही नहीं रह गया है, ऐसा कोई सहारा नहीं बचा जिसे थामकर चला जा सके, कोई धर्म ही नहीं रहा। मानसिक सत्ता में जो कर्म तत्त्व अथवा कर्म-पुरुष है उसके लिए यह सबसे भयंकर संकटावस्था, विफलता तथा पराभव है। स्वयं यह विद्रोह अत्यंत सहज और स्वाभाविक है; संवेदनात्मक रूप से विद्रोह ऐसे कि, इसमें भय, दया और जुगुप्सा के बिल्कुल सामान्य भाव हैं, प्राणिक रूप से विद्रोह ऐसे कि, जीवन के उद्देश्यों और कर्म के सर्वस्वीकृत एवं सुपरिचित हेतुओं में आकर्षण और श्रद्धा न रहना, भावावेगात्मक रूप से विद्रोह ऐसे कि, सामाजिक मानव की सामान्य भावनाओं जैसे स्नेह, आदर-सत्कार, सम्मिलित प्रसत्रता व संतुष्टि की कामना - का एक निर्मम कर्तव्य से पीछे हटना जो उन सभी भावनाओं का उल्लंघन करने वाला है; नैतिक रूप से ऐसे कि, पाप और नरक का अतिसामान्य भाव तथा 'रक्तरंजित भोगों' के निषेध का 'भाव; व्यावहारिक रूप से, यह बोध कि कर्म के मानदण्ड एक ऐसे परिणाम तक ले आए हैं जो कर्म के व्यावहारिक उद्देश्यों को ही नष्ट कर देता है।
इसमें बात बड़ी स्पष्ट है। जब तक मनुष्य के जीवन में परस्पर-विरोधी कर्तव्य-अकर्तव्य की स्थिति पैदा नहीं हो जाती, तब तक जो भी भाव प्रधान रूप से प्रभावी रहता है उसी के अनुसार सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहता है। परन्तु संकट तो तब पैदा होता है जब ऐसी परिस्थिति आ खड़ी होती है जिसमें परस्पर विरोधी कर्त्तव्य उपस्थित हो जाते हैं और दोनों का ही दावा शक्तिशाली होता है। अब यहाँ अर्जुन के समक्ष अनेक धर्म एक दूसरे के विरोध में आ खड़े हुए हैं- अधर्म पर विजय के लिए लड़े, क्षत्रिय धर्म का पालन करे, या अपने गुरुओं के प्रति कर्त्तव्य का पालन करे या उनका संहार करने का पाप करे। ऐसी परिस्थिति में कौन से कर्तव्य का पालन करे। ऐसे में जो मनुष्य मानसिक आदर्शों के अनुसार कर्म करता है वह स्वाभाविक रूप से इस चयन में दुविधा अनुभव करेगा कि कौनसे आदर्श का अनुसरण करे। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। उसका इन्द्रियबोध एक बात कहता है, भावात्मकता दूसरी बात, नैतिकता तीसरी बात और कर्त्तव्य कर्म की भावना एक अलग ही बात कहती है। और इसी संकटावस्था से गीता का जन्म होता है। इसके समाधान के रूप में गीता हमें उस उच्च स्थल तक ले जाएगी जहाँ इन सब प्रश्नों का महत्त्व ही नहीं रहेगा, जहाँ इस तरह के भिन्न कर्तव्यों का अंतर्विरोध समाप्त हो जाएगा और बुद्धि में स्पष्टता आ जाएगी। जब कोई योग मार्ग में चलता है तो उसके लिए केवल एक ही कर्तव्य रह जाता है और वह है वही कर्म करना जिसमें श्रीमाताजी (या भगवान्) की प्रसन्नता निहित हो। किंतु चूंकि इस विषय में अंधकार रहता है कि 'उन्हें' कौनसी चीज प्रसन्न करेगी, इसलिए व्यक्ति कर्तव्यबोध का सहारा लेता है। परंतु ऐसे में यात्रा कभी भी अपनी पूर्णाहुति तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि यात्रा में व्यक्ति कभी सही मोड़ ले लेता है तो कभी गलत। सामान्यतः साधना में ऐसा ही होता है और इस कारण अधिकतर लोग एक ही जगह पर चक्कर काटते रहते हैं। इस सब से हमें यह सबक लेना चाहिये कि बिना सच्चे मार्गदर्शन के साधना में सफलता संभव नहीं है।
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्वितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ।।७।।
७. कार्पण्य दोष (दुर्बलता) ने मुझसे मेरा (सच्चा वीरोचित) क्षत्रिय स्वभाव छीन लिया है, धर्म-अधर्म (कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य) के निर्णय करने में मेरी संपूर्ण चेतना विमूढ़ हो गयी है, इसलिये मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिये श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बतलाइये; मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, मुझे ज्ञानोद्दीप्त कीजिये।
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्।
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ।।८।।
८. क्योंकि पृथ्वी पर समृद्ध और निष्कंटक राज्य अथवा देवताओं के ऊपर आधिपत्य (स्वर्ग के ऊपर राज्य) के प्राप्त हो जाने पर भी मैं ऐसा कोई साधन नहीं देखता जो मेरी इन्द्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके।
सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा इषीकेशं गुडाकेशः परंतप ।
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ।९।।
९. सञ्जय ने कहाः हे परंतप (घृतराष्ट्र), इषीकेश से इस प्रकार कह देने के बाद, गुडाकेश (निद्राजयी अर्जुन) उन गोविन्द से "मैं युद्ध नहीं करूंगा" इस प्रकार कह कर चुप हो गया।
अर्जुन श्रीकृष्ण को दिये अपने उत्तर में फटकार को स्वीकार करता है, जबकि अभी भी वह उनके आदेश पालन में आनाकानी करता है और इन्कार कर देता है। वह अपनी दुर्बलता को जानता है, फिर भी उसकी अधीनता स्वीकार करता है। उसकी कार्पण्यता (दुर्बलता) ने उससे उसके सच्चे वीर स्वभाव को छीन लिया है, उसकी सारी चेतना धर्मसंमूढ़ (किंकर्तव्यविमूढ़) हो गयी है और वह अपने दिव्य सखा को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है; परन्तु जिन भावावेगमय और बौद्धिक आधारों पर उसने अपनी धर्मपरायणता के बोध को आश्रित किया था, उन्हें सर्वथा गिरा दिया गया है और वह एक ऐसे आदेश को स्वीकार नहीं कर सकता जो उसके अनुसार उसके पुराने दृष्टिकोण के जैसा ही है और कर्म करने के लिए कोई नया आधार प्रदान नहीं करता। इसलिए अभी भी वह प्रस्तुत कर्म के लिए अपनी अस्वीकृति को उचित ठहराने की चेष्टा करता है और उसके समर्थन में अपनी स्नायवीय और संवेदनात्मक सत्ता के दावे को प्रस्तुत करता है जो इस संहारकर्म से और इसके परिणाम के रूप में रक्त से सने हुए भोगों से काँपती है, अपने हृदय के दावे को प्रस्तुत करता है जो उसके इस कृत्य के बाद आने वाले शोक और जीवन की रिक्तता से काँपता है, अपने प्रचलित नैतिक धारणाओं के दावे को प्रस्तुत करता है जो भीष्म और द्रोणाचार्य सरीखे गुरुजनों का वध करने की अनिवार्यता से भयभीत अथवा स्तंभित हैं, अपनी तर्कबुद्धि के दावे को प्रस्तुत करता है जो उसको सौंपे गये भीषण और प्रचण्ड कर्म में कोई भी भलाई नहीं देखती, अपितु जिसमें उसे अशुभ अथवा बुरे परिणाम ही नजर आते हैं। वह दृढ़-प्रतिष्ठ है कि (युद्धसंबंधी) विचार और हेतु के पुराने आधार पर वह नहीं लड़ेगा और फिर वह अपनी आपत्तियों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, जिनका कि (उसकी समझ में) कोई उत्तर नहीं हो सकता। अर्जुन की अहंपरक सत्ता के इन्हीं दावों को श्रीकृष्ण सर्वप्रथम नष्ट करना शुरू करते हैं ताकि उस उच्चतर धर्म के लिये स्थान बनाया जा सके जो कर्म के समस्त अहंपरक हेतुओं का अतिक्रमण करेगा।
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ।।१०।।
१०. हे भारत (धृतराष्ट्र) ! दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से श्रीकृष्ण ने मानो हँसते हुए ये वचन कहे।
श्रीगुरु का उत्तर दो विभिन्न धाराओं पर चलता है। पहला संक्षिप्त उत्तर उस सामान्य आर्य-संस्कृति की उच्चतम धारणाओं पर आधारित है जिसमें कि अर्जुन पला-बढ़ा है, उसने शिक्षा-दीक्षा ली है, दूसरा, सर्वथा भिन्न प्रकार का और अधिक व्यापक है, जो कि एक अधिक अंतरंग ज्ञान पर आधारित है जो कि हमारी सत्ता के गंभीरतर सत्यों की ओर खुलता है, और वही ज्ञान गीता की शिक्षा का वास्तविक आरंभ-बिंदु है। पहला उत्तर वेदांत दर्शन की दार्शनिक और नैतिक धारणाओं पर तथा कर्त्तव्य और स्वाभिमान-संबंधी उस सामाजिक भाव पर आश्रित है जिससे आर्यों के समाज का नैतिक आधार बना था।
श्रीभगवान् उवाच
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्व भाषसे ।
गतासूनगतासुंश्व नानुशोचन्ति पण्डिताः ।।११।।
११. श्रीभगवान् ने कहाः जिनके लिये शोक करना उचित नहीं है उनके लिये तू शोक करता है और फिर भी ज्ञानी के जैसी बातें कहता है, किंतु जो ज्ञानी है वह न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करता है।
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ।।१२।।
१२. मैं किसी भी समय नहीं था ऐसा नहीं है, तू नहीं था ऐसा भी नहीं है, ये राजा लोग नहीं थे यह भी सही नहीं है; और हम सब लोग यहाँ से प्रयाण करने पर नहीं रहेंगे यह भी नहीं है।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्षीरस्तत्र न मुह्यति ।।१३।।
१३. जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस देह में कौमार, यौवन और वृद्धावस्था से गुजरती है, उसी प्रकार उसे इस देह से दूसरे देह की प्राप्ति होती है; इस विषय में धीर और विवेकी मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होता।
अर्जुन ने अपनी अस्वीकृति को नैतिक और यौक्तिक आधारों पर उचित ठहराने की चेष्टा की है, परंतु इसमें उसने महज अपने अज्ञानी और अशुद्ध भावावेगों के विद्रोह को युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले शब्दाडंबर से ढका भर है। उसने भौतिक जीवन और शरीर की मृत्यु के संबंध में इस प्रकार कहा है मानो ये ही प्रमुख यथार्थताएँ हों; परन्तु ज्ञानी और पंडितों की दृष्टि में इनका ऐसा कोई मूलभूत महत्त्व नहीं है। अपने मित्रों और बंधुओं की शारीरिक मृत्यु का दुःख एक ऐसा शोक है जिसे प्रज्ञा अथवा विवेक और जीवन का सच्चा ज्ञान कोई स्वीकृति नहीं प्रदान करते। ज्ञानी पुरुष किसी जीवित अथवा मृत के लिए शोक नहीं किया करता, क्योंकि वह जानता है कि दुःख और मृत्यु आत्मा के इतिहास में घटनाएँ मात्र हैं। आत्मा, न कि शरीर, ही यथार्थता है। ये सब मनुष्यों के राजागण, जिनकी आनेवाली मृत्यु के लिए अर्जुन शोक कर रहा है, इस जीवन के पहले भी जीये हैं और आगे भी मानव-देह में जीयेंगे; क्योंकि जैसे आत्मा शारीरिक रूप से कौमार, यौवन तथा वार्द्धक्य की अवस्था से गुजरती है वैसे ही वह शरीर-परिवर्तन करती है। शांत तथा विवेकी बुद्धि से युक्त, जो धीर है, विचारक है, जो जीवन को स्थिरतापूर्वक देखता है और अपने-आप को इन्द्रियानुभवों और भावावेगों से विक्षुब्ध और अंधा नहीं होने देता, वह भौतिक प्रतीतियों से धोखा नहीं खाता; वह अपने खून के, अपनी स्नायुओं के तथा अपने हृदय के कोलाहल को अपने निर्णय का आच्छादन अथवा अपने ज्ञान का खण्डन नहीं करने देता। वह शरीर और इन्द्रियों के जीवन के बाह्य तथ्यों के परे जाकर अपनी सत्ता के वास्तविक तथ्य को देखता है और अपनी अज्ञानमय प्रकृति की भावावेगमय और भौतिक कामनाओं से ऊपर उठकर मानव-जीवन के सच्चे और एकमात्र ध्येय में पहुँच जाता है।
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ।।१४।।
१४. हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! भौतिक पदार्थों के (इन्द्रियों के साथ) जो स्पर्श (संयोग) होते हैं वे शीत ऊष्ण, सुख और दुःख देनेवाले हैं, और वे अनित्य होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं; हे भारत उनको तू सहन करना सीख ।
इन चीजों को तब तक सहन करना होगा जब तक इन पर विजय न प्राप्त कर ली जाए, जब तक कि ये मुक्त पुरुष को कोई दुःख न दे सकें, जब तक कि संसार की सब पार्थिव घटनाओं को, चाहे सुखद हों या दुःखद, वह ज्ञानयुक्त और स्थिर समता से वैसे ही ग्रहण न कर सके जैसे हमारे अन्दर गूढ़ शांत सनातन आत्मा उन्हें ग्रहण करती है। शोक और भय से विचलित होना, जैसे अर्जुन हुआ है, और अपने गंतव्य पथ से भ्रष्ट हो जाना, तथा दैन्य और दुःखभार से दबकर शारीरिक मृत्यु की अनिवार्य और अतिसामान्य घटना का सामना करने से पीछे हटना 'अनार्यजुष्टं' अनार्य अज्ञान है। यह उस आर्य का मार्ग नहीं है जो धीर शक्ति के साथ अमर जीवन की ओर ऊपर चढ़ता रहता है।
ⅱ.2
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।।१५।।
१५. हे पुरुषों में श्रेष्ठ (अर्जुन)! जिस मनुष्य को ये स्पर्श व्यथित नहीं करते, जो धीर-स्थिर विवेकी मनुष्य दुःख और सुख में समान रहने वाला है वह अपने-आप को अमृतत्व के योग्य बना लेता है।
...जगत् के महान् चक्रों के भीतर युगों-युगों के द्वारा पुनरावर्तित होते मनुष्य के जीवन और मरण केवल एक ऐसी दीर्घ कालव्यापी प्रगति हैं जिनके द्वारा मानव-प्राणी अपने-आपको तैयार करता है और अमृतत्व के लिये योग्य बनाता है। और वह अपने-आपको कैसे तैयार करे? कौन-सा मनुष्य योग्य होता है? वह व्यक्ति जो अपने-आपको प्राण और शरीर समझने वाली धारणा से ऊपर उठ जाता है, जो संसार के भौतिक और संवेदनात्मक संपकों को उनके अपने मूल्य पर, अथवा देहात्मबुद्धि वाले लोग उसे जो मूल्य प्रदान करते हैं उस पर, उन्हें स्वीकार नहीं करता, जो स्वयं को और सभी को आत्मा जानता है, जो अपने-आप को अपने शरीर में नहीं, अपितु आत्मा में निवास करने का अभ्यासी बना लेता है और दूसरों के साथ भी आत्मा के रूप में, न कि उन्हें मात्र दैहिक प्राणी जानकर, व्यवहार करता है। क्योंकि अमृतत्व का अर्थ मृत्यु से बचे रहना नहीं है - वह तो एक मन से युक्त होकर जन्मे प्रत्येक प्राणी को पहले से ही प्राप्त है, अपितु जीवन और मरण को अतिक्रम करना, उनके परे चले जाना है। इसका अभिप्राय उस आरोहण या ऊर्ध्व-गति से है जिससे मनुष्य मन से अनुप्राणित शरीर के रूप में न रहकर अंततः एक आत्मा के रूप में और 'आत्मा' के अंदर निवास करता है। जो कोई शोक और दुःख के अधीन है, इन्द्रियानुभवों और भावावेगों का दास है, क्षणभंगुर और अनित्य पदार्थों के स्पर्शों में लिप्त रहता है, वह अमृतत्व का अधिकारी नहीं हो सकता।
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।।१६।।
१६. जो वस्तुतः सत् है उसका अभाव नहीं हो सकता, वैसे ही जैसे जो असत् है उसकी विद्यमानता नहीं हो सकती। तथापि इन दोनों सत् और असत् के विरोधों का ही अंत तत्त्वदर्शियों द्वारा देखा गया है।
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्वित्कर्तुमर्हति ।।१७।।
१७. किंतु जिस आत्मा से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है उसे तू अविनाशी समझ। इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ।।१८ ।।
१८. उस शरीरधारी आत्मा के, जो नित्य, अविनाशी और अपरिमेय है, ये समस्त शरीर अंतवंत अर्थात् विनाशवान कहे गये हैं; इसलिये हे भारत (अर्जुन) ! युद्ध कर।
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।१९।।
१९. जो मनुष्य इसे (आत्मा को) हत्या करने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है वे दोनों ही सत्य को नहीं देख पाते। न यह किसी की हत्या करता है न हत ही होता है।
न जायते नियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।।२०।।
२०. यह (आत्मा) कभी उत्पन्न नहीं होता और न मरता ही है, और न यह कोई ऐसा पदार्थ ही है जो एक बार अस्तित्व धारण कर के (चले जाने पर) फिर कभी भी अस्तित्व न धारण कर सकता हो। यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है, शरीर की हत्या होने के साथ यह हत नहीं होता।
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ।।२१।।
२१. हे पार्थ ! जो मनुष्य इस (आत्मा) को अजन्मा, अव्यय, नित्य, अविनाशी जानता है वह मनुष्य किस प्रकार किसी की हत्या करता है अथवा किसी की हत्या का कारण बनता है?
वासांसि जीर्णानि यथा विहायनवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥
२२. जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग कर के दूसरे नवीन वलों को ग्रहण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों का परित्याग कर के दूसरे नवीन शरीरों को धारण करता है।
नैनं छिन्दन्ति शखाणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।॥२३॥
२३. इस आत्मा को शत्र काट नहीं सकते, न ही अग्नि जला सकती है, और न इसे जल गीला कर सकते हैं, और न हवा इसे सुखा सकती है।
अच्छेद्यो ऽयमदाह्यो ऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।।२४।।
२४. यह आत्मा कभी भी न कट सकने वाला, न जल सकने योग्य, न गीला हो सकने वाला और कभी भी न सुखाया जा सकने वाला है; यह शाश्वत रूप से नित्य, अचल, सर्वव्यापी और सनातन है।
अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो ऽयमविकार्यो ऽयमुच्यते ।
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ।।२५।।
२५. यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य, अविकारी है, ऐसा (श्रुतियों द्वारा) इसका वर्णन है; इसलिये इस आत्मा को इस प्रकार के स्वरूप वाला जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिये।
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ।।२६।।
२६. और यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म ग्रहण करने वाला और निरंतर मरणशील (ही) मानता है तब भी हे महाबाहो अर्जुन ! तेरा इसके विषय में शोक करना उचित नहीं है।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ।।२७॥
२७. क्योंकि पैदा हुए का मरण निश्चित है और मृत का फिर जन्म ग्रहण करना निश्चित है; इसलिये जो अपरिहार्य है उसके विषय में तेरा शोक करना उचित नहीं है।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना । ॥२८॥
२८. हे भारत! समस्त प्राणी आदि में अव्यक्त होते हैं, मध्य में व्यक्त होते हैं, निधनोपरान्त वे फिर अव्यक्त हो जाते हैं, इसलिये इसमें शोक करने की क्या बात है?
भौतिक मन और इन्द्रियों द्वारा मृत्यु के विषय में तथा मृत्यु के भय में, चाहे वह मृत्यु रोग-शय्या पर हो या रणक्षेत्र में, जो रोना-पीटना होता है वह प्राण की चीत्कारों में सबसे अधिक अज्ञानमय है। मनुष्यों की मृत्यु के प्रति हमारा शोक उन लोगों के लिये अज्ञानी रूप से दुःख करना है जिनके लिये दुःख करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि न तो वे अस्तित्व से बाहर गये हैं न उनकी अवस्था में कोई दुःखद या भयानक परिवर्तन ही हुआ है क्योंकि मृत्यु के परे वे कोई कम सत्ता में नहीं हैं और उस अवस्था में जीवन की अपेक्षा कोई अधिक दुःखी नहीं हैं।
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः ।
आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ।।२९।।
२९. कोई मनुष्य इसे (आत्मा को) आश्चर्यमय रूप में देखता है, कोई दूसरा मनुष्य आश्चर्यवत् इसका वर्णन करता है; और कोई दूसरा आश्चर्यमय रूप में इसका श्रवण करता है और सुनने के पश्चात् भी इसे (आत्मा को) कोई नहीं जानता।
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ।।३०।।
३०. हे भारत! सबकी देहों में यह आत्मा नित्य है और अवध्य है; इसलिये तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
केवल एक ही चीज सत्य है जिसमें हमें रहना होगा, (वह है) अपनी यात्रा के महान् चक्र में मानव-आत्मा (जीव) के रूप में उस शाश्वत पुरुष का स्वयं को प्रकट करना, जिस यात्रा में जन्म और मृत्यु मार्ग में मील के पत्थर हैं (महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं), जहाँ परलोक विश्राम-स्थल-स्वरूप हैं, जिसमें जीवन की सारी अवस्थाएँ, चाहे सुखद हों या दुःखद, हमारी प्रगति, संग्राम और विजय के साधन हैं तथा अमरत्व हमारा धाम है जिसके लिये आत्मा यात्रा करती है...
यह उच्च और महान् ज्ञान, मन और आत्मा का यह कठोर स्व-अनुशासन जिसके द्वारा उसे भावावेगों की चीत्कार और इन्द्रियों के धोखों के परे सच्चे आत्मज्ञान में ऊपर उठना है, जो हमें शोक और भ्रम से मुक्त कर सकता है...हमें भली प्रकार जीवन के भयंकर थपेड़ों को अक्षुब्ध अथवा अविचल भाव से देखना और शरीर की मृत्यु को एक तुच्छ या नगण्य घटना के तौर पर देखना सिखा सकता है... परंतु इससे अर्जुन से जिस कर्म की माँग की जा रही है, तथा कुरुक्षेत्र का जो संहारकर्म है, उसे कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि अर्जुन को जिस पथ पर चलना है वह पथ इस कर्म की माँग करता है; यह कर्म उसके अपने स्वधर्म सामाजिक कर्तव्य, जीवनधर्म और अपनी सत्ता के धर्म द्वारा अपेक्षित कर्त्तव्य के निर्वाह में अपरिहार्य रूप से आ पड़ा है।
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।
धर्माद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ।।३१।।
३१. और फिर, अपने स्वधर्म को देखते हुए भी तुम्हें (अपने युद्धरूप कर्म से) विचलित नहीं होना चाहिये; क्योंकि क्षत्रिय के लिये धर्मयुद्ध से बढ़कर अन्य कोई चीज श्रेष्ठ नहीं है।
इसके बाद गुरु क्षण भर के लिये विषय से अलग हटकर आत्मीय-स्वजनों की मृत्यु से होनेवाले उस दुःख संबंधी विलाप का एक और उत्तर देते हैं, (अर्जुन के अनुसार) जिनकी मृत्यु उसके जीवन को जीने के कारणों और हेतुओं से ही रिक्त कर देगी। क्षत्रिय के जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है और उसका सच्चा सुख क्या है? यह अपने-आपको खुश करना, पारिवारिक सुख देखना और मित्रों और सगे-संबंधियों के साथ सुखकर और शांत हर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करना नहीं है अपितु धर्म के लिये लड़ना ही उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य है, और उसका महत्तम सुख होगा कोई ऐसा महत्-कार्य या उद्देश्य खोज निकालना जिसके लिए वह अपना जीवन उत्सर्ग कर सके या फिर विजयी होकर राज्य तथा वीरोचित जीवन का यश और गौरव प्राप्त करे।
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ।।३२॥
३२. हे पार्थ। वे क्षत्रिय सुखी (भाग्यशाली) होते हैं जब ऐसा युद्ध स्वयं उनके पास स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान चला आता है।
अथ चेत्त्वमिमं धम्यै संग्रामं न करिष्यसि ।
ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।। ३३ ।।
३३. किन्तु यदि तू इस युद्ध को धर्म के हेतु नहीं करेगा, तो स्वधर्म को और अपनी कीर्ति को खो बैठेगा और पाप का भागी बनेगा।
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥
३४. इसके अतिरिक्त, मनुष्य तेरी दीर्घ काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहेंगे, और महिमान्वित मनुष्य के लिये अपकीर्ति मरने से भी अधिक बुरी है।
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ।।३५।।
३५. महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे और तू जो अभी तक उनकी दृष्टि में बहुत अधिक माननीय रहा है अब उनकी दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाएगा।
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ।।३६।।
३६. तेरे शत्रु तेरे बल की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे; इससे अधिक दुःखदायी और क्या हो सकता है?
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।॥३७॥
३७. यदि तू मारा जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा; यदि विजयी होता है तो पृथ्वी का भोग करेगा; इसलिये हे कुन्तीपुत्र (अर्जुन)! युद्ध करने का निश्चय कर के खड़ा हो।
यह वीरोचित आग्रह इससे पूर्व चर्चा की गई निस्पृह आध्यात्मिकता से तथा आगे आने वाली गंभीरतर आध्यात्मिकता से निचले स्तर का प्रतीत हो सकता है; क्योंकि अगले ही श्लोक में श्रीगुरु अर्जुन को सुख-दुःख, लाभ-अलाभ और जय-पराजय में समता बनाये रखकर युद्ध करने का निर्देश देते हैं और यही गीता का वास्तविक उपदेश है। परन्तु भारतीय नीतिशास्त्र ने मनुष्य के विकासोन्मुख नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए क्रमोन्नत आदर्शों की व्यावहारिक आवश्यकता को सदा ही अनुभव किया है। यहाँ क्षत्रिय का जो आदर्श सामने रखा गया है वह चातुर्वर्ण्य के अनुसार सामाजिक दृष्टि से रखा गया है, इसकी जो आध्यात्मिक दृष्टि आगे चलकर दिखायी गयी है उस दृष्टि से नहीं। श्रीकृष्ण यहाँ अर्जुन से वास्तव में यही कह रहे हैं कि 'यदि तू सुख और दुःख और कर्म के परिणाम को ही अपने कर्म के हेतु के रूप में मानने पर आग्रह रखता है तो मेरा तुझे यही उत्तर है। मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि आत्मा और जगत् का जो उच्चतर ज्ञान है वह तुझे किस दिशा में प्रवृत्त करता है; और अब मैंने यह भी दिखाया है कि तेरा सामाजिक कर्त्तव्य और तेरी जाति या वर्ण का अपना नैतिक आदर्श तुझे किस दिशा में प्रवृत्त करता है; 'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य।' तू जिस किसी भी पहलू से देख, परिणाम एक ही है। परन्तु, यदि तू अपने सामाजिक कर्तव्य और वर्णधर्म से संतुष्ट न होता हो, और समझता हो कि उससे तू दुःख और पाप का भागी बनेगा तो मेरा आदेश है कि किसी हीन आदर्श की ओर नीचे गिरने की अपेक्षा किसी ऊँचे आदर्श की ओर ऊपर उठ ।'
इसमें श्रीअरविन्द ने अपनी टीका में जो तर्क दिया है उसमें तीन बातें हैं। इसके अंदर अर्जुन यह तर्क देता है कि 'माना कि विरोधी पक्ष के लोग तो भ्रमित हैं, मूढ़ हैं, परन्तु हमें तो समझ है। आखिर इस युद्ध से क्या होगा? सभी लोग नष्ट हो जाएँगे। मेरे गुरुजन और पितामह, जिन्होंने मुझे इतनी शिक्षा, इतना ज्ञान दिया है, उनके प्रति युद्ध करके तो मुझे रक्त में सने हुए भोगों के अतिरिक्त और क्या मिलने वाला है? तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। तो फिर ये सुख-भोग तो तुच्छ-सी चीजें हैं, इनके लिए तो मेरा इन्हें मारने का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे हमारा कुलधर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे पितरों का तर्पण नहीं होगा और सब अनिष्ट हो जाएगा।' इस सब तर्क पर श्रीकृष्ण ने जो उत्तर दिया उसे कहते हैं 'आर्य-क्षत्रिय का धर्ममत।' जिस रूप में हिन्दुस्तान के घर-घर में वेदान्त के विचार प्रचलित हैं कि भगवान् सब जगह हैं, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, वह अमर है, आदि-आदि, ऐसे ही प्रचलित विचारों के सहारे उसे उत्तर दिया जा रहा है कि 'वह बातें तो पण्डितों के समान करता है कि हमें यह करना चाहिये अथवा यह नहीं करना चाहिये, परन्तु पण्डित-जन तो जो जीवित हैं या जो मर गए हैं, उनमें से किसी के लिए शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में जीवित और मृत के बीच में कोई अन्तर नहीं होता। आत्मा तो अमर है, न कभी ये मरती है, न कभी इसका कुछ बिगड़ सकता है। संसार तो अनित्य है और ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले नहीं थे और महाभारत के बाद नहीं रहेंगे, इसलिए वह किसके लिए शोक करता है।' हालाँकि अर्जुन अपने मुँह से यह प्रश्न नहीं करता, किन्तु यहाँ प्रश्न उठता है कि माना कि ये सब अनित्य हैं, इनकी मृत्यु तो होनी ही है और आत्मा अमर है, परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि इन सब को वह मार डाले। यह बात तो आध्यात्मिकता नहीं कहती कि चूंकि शरीर अनित्य है इसलिए इन्हें मार डालना चाहिये। आर्य क्षत्रियों के धर्म की बात तो उचित है परन्तु संहार-कर्म को यहाँ उचित कैसे ठहराया जाए? इसका उत्तर यह है कि भले आध्यात्मिकता के अनुसार तो जन्म और मृत्यु समान ही हैं, इसलिए मारो या नहीं मारो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु चूँकि यह परिस्थिति उसके सामने उपस्थित हुई है इसलिए उसे अपने क्षात्र-धर्म का पालन करना चाहिये क्योंकि क्षत्रिय अपने निजी सुख-दुःख से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता। उसे तो सदा ही सही के लिए लड़ना चाहिए और सत्य के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देना चाहिये। और ऐसा ही एक अवसर आज उसके सामने उपस्थित है। ऐसे युद्ध में यदि वह जीतता है तो राज्य करेगा और मृत्यु को प्राप्त होता है तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। और यदि वह इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता है तो यह उसके क्षत्रिय धर्म के अनुरूप कर्म नहीं होगा। इसलिये यदि वह यह तर्क देता है कि युद्ध करने से उसे तकलीफ होगी, तो उसे यह भी विचार करना चाहिये कि युद्ध से परे हटने के कारण लोग उसे कायर कहेंगे और उससे जो उसकी अपकीर्ति होगी वह तो उसके लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगी। इससे तो वह वीरतापूर्वक युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हो तो ज्यादा अच्छा है। और यदि वह आध्यात्मिकता की बात करता है, कि आत्मा अमर है, शरीर अनित्य है, तो भी उसके लिए यही कर्म करना सही है। किसी भी तरह से उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसे जय-पराजय को समान मानकर युद्ध करना चाहिये। परंतु अर्जुन कहता है कि 'यदि मैं इन्हें समान ही मानूँ, और इनसे अप्रभावित रहूँ तो फिर मैं लडूं ही क्यों? आखिर मुझे लड़ना ही क्यों चाहिये?' और सतही तौर पर इस तर्क का क्या समाधान हो सकता है? भगवान् इसका बिल्कुल सीधा उत्तर देते हैं कि क्योंकि 'मैं ऐसा करने को कह रहा हूँ और ऐसी मेरी इच्छा है' और 'मैं ही एकमात्र हूँ जिसका कि अस्तित्व है इसलिए मेरी इच्छा पूरी करना ही तेरा काम है, अतः यज्ञ के रूप में कर्म कर।' वास्तव में इसके अतिरिक्त और कोई उत्तर हो भी नहीं सकता। श्रीअरविन्द ने अपनी टीका में जिस तरीके से इस तर्क को विकसित किया है वैसा हमें सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। उसके बिना तो हम इससे चूक ही जाते हैं कि इसमें तीन तरीके के तर्क भी हैं। अब अर्जुन निरुत्तर हो जाता है। पर वह पूछता है कि जय-पराजय, सुख-दुःख सबको समान मानकर निष्काम कर्म करना संभव ही कैसे है? बिना किसी कामना के या ऐसा भाव अपनाकर व्यक्ति किस आधार पर कर्म का चुनाव कर सकता है? उसी के उत्तरस्वरूप श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'यज्ञ के रूप में और मेरी प्रसन्नता के निमित्त कर्म कर।' तब फिर अर्जुन पूछता है कि 'आप कौन हैं।' और इसी का उत्तर उन्होंने नौंवें, दसवें और ग्यारहवें अध्याय में दे दिया कि वे कौन हैं, उनका स्वरूप क्या है। यही गीता का इस सारी समस्या का समाधान है, कि समस्या कर्तव्य या अकर्त्तव्य की नहीं है, सारी बात तो यह है कि भगवान् ही सब कुछ हैं, और वे जो कहें वही सही है। इसमें व्यक्ति के तर्क, उसके धर्म-अधर्म, दर्शन आदि के सिद्धांतों को उचित-अनुचित की क्या समझ है? इसकी वास्तविक समझ तो केवल भगवान् को ही है।
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।। ३८ ।।
३८. सुख-दुःख, लाभ-अलाभ और जय-पराजय में समता रख और तब युद्ध कर; इससे तू पाप को प्राप्त नहीं होगा।
इस प्रकार अर्जुन की जो विषादजनित दलीलें थीं, संहारकर्म से पीछे हटने की जो दलीले थीं, पापबोधजन्य दलीलें तथा कर्म के दुष्परिणाम की आशंका की दलीलें थीं उन सबका उत्तर, अर्जुन की जाति और युग के उच्चतम ज्ञान और श्रेष्ठ नैतिक आदर्श के अनुसार दिया जा चुका है।
अब हमें देखना है कि अर्जुन की कठिनाई और इन्कार के मूल में जो समस्या है उसके दृष्टिकोण से तथा अत्यंत स्पष्ट और निश्चयात्मक शब्दों में इस समाधान का क्या अभिप्राय है। एक मनुष्य तथा सामाजिक प्राणी के रूप में उसका कर्त्तव्य क्षत्रिय के उच्च धर्म का पालन करना है जिसके बिना समाज के ढाँचे की रक्षा नहीं की जा सकती, जाति के आदर्शों को न्यायसंगत सिद्ध नहीं किया जा सकता, और अत्याचार, पाप और अन्याय के अराजक उत्पात के विरुद्ध धर्म और न्याय की सुसमंजस व्यवस्था को धारण नहीं किया जा सकता। और फिर भी कर्तव्य का आह्वान अपने-आप में युद्ध के नायक को अब पहले की तरह संतुष्ट नहीं कर सकता क्योंकि कुरुक्षेत्र की भीषण यथार्थता के बीच वह आह्वान अपने-आप को अति कठोर, विमूढ़कारी और अस्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। अपने सामाजिक कर्त्तव्य का निर्वाह उसके लिए सहसा ही उस अर्थ का द्योतक हो गया है कि वह अपरिमित पाप तथा दुःख-कष्टरूपी परिणाम के लिए अपनी सहमति दे, सामाजिक व्यवस्था और न्याय को बनाए रखने के परंपरागत साधन उल्टे बड़ी भारी अव्यवस्था और अराजकता की ओर ले जाने वाले हो रहे हैं। न्यायोचित दावों और अधिकार का नियम, जिसे न्याय्य अधिकार कहते हैं, यहाँ उसकी कोई सहायता नहीं करेगा; क्योंकि जो राज्य उसे अपने लिए, अपने बंधु-बांधवों तथा युद्ध में अपने पक्ष के लोगों के लिए जीतना है उस पर वास्तव में न्यायपूर्वक उन्हीं का अधिकार है तथा उस अधिकार की बलपूर्वक स्थापना करने का अर्थ आसुरी अत्याचार का उन्मूलन और न्याय का प्रतिष्ठापन करना है, परंतु वह न्याय रक्त-रंजित न्याय होगा और वह राज्य एक ऐसा राज्य होगा जो शोकाकुल हृदय के साथ अधिकृत होगा जिस पर एक महापाप, समाज की भयंकर हानि और जाति के प्रति ज्वलंत अपराध का कलंक होगा। और न ही धर्म, अर्थात् नैतिक धर्म, का विधान ही कोई सहायता करने वाला है; क्योंकि यहाँ धर्मों का परस्पर विरोध उपस्थित है। इस समस्या के समाधान के लिए एक नवीन तथा महत्तर परंतु अब तक के किसी भी अनुमान से परे के विधान की आवश्यकता है, परन्तु वह विधान है क्या?
क्योंकि अपने कर्म से अलग हट जाना, साधुओं के जैसी अकर्मण्यता का सहारा ले लेना तथा असंतोषकर तरीकों और हेतुओं से युक्त इस अपूर्ण संसार को उसके अपने ही साधनों के भरोसे त्याग देना इस समस्या का एक सहज ही कल्पनीय संभव समाधान है, जिसे लागू करना भी आसान है परंतु यह तो ठीक उस ग्रंथिमात्र को ही काट देना होगा जिसकी श्रीगुरु ने बलपूर्वक मनाही की है। किन्तु इस जगत् के स्वामी, जो मनुष्य के सब कमर्मों के स्वामी हैं और यह जगत् जिनकी एक कर्मभूमि है, द्वारा मनुष्य से कर्म की माँग की जाती है, भले वह कर्म अहंभाव के द्वारा तथा सीमित मानव बुद्धि के अज्ञान या आंशिक प्रकाश में किया जाए या फिर यह अंतर्दर्शन तथा प्रेरणा के एक अधिक उच्च तथा अधिक व्यापक दृष्टि वाले स्तर से प्रवर्तित हो। और फिर, इस (संहार) कर्म विशेष को अमंगलकारी बताकर इसका परित्याग कर देना एक दूसरे प्रकार का समाधान होगा जो कि अदूरदर्शी नैतिकतावादी अथवा उपदेशात्मक मन का बना-बनाया उपाय है, परंतु इस प्रकार की टाल-मटोल के लिए भी श्रीगुरु अपनी सहमति अस्वीकार कर देते हैं। अर्जुन की कर्म से निवृत्ति एक और अधिक बड़े पाप और बुराई का कारण बनेगी: यदि इसका कुछ परिणाम हुआ भी तो वह होगा अन्याय और अनाचार की विजय तथा भगवत्कार्यों के यंत्ररूप बने रहने के उसके अपने ही महाव्रत का परित्याग। जाति की भवितव्यताओं में जो प्रचंड संकट उत्पन्न हो गया है वह शक्तियों की कोई अंध गति या मात्र मानवीय विचारों, स्वार्थों, आवेगों तथा अहंकारों के अस्तव्यस्त संघर्ष के कारण नहीं उत्पन्न हुआ है अपितु एक भगवदिच्छा द्वारा लाया गया है जो इन बाह्य प्रतीतियों के पीछे कार्य कर रही है। अर्जुन को अवश्य ही इस सत्य का साक्षात्कार करा देना होगा; उसे अपनी क्षुद्र व्यक्तिगत कामनाओं तथा दुर्बल मानवीय जुगुप्साओं के यंत्र के रूप में नहीं अपितु एक बृहत्तर तथा अधिक ज्योतिर्मयी शक्ति, एक महत्तर सर्वज्ञ, दिव्य और वैश्व संकल्प के यंत्र के रूप में, निर्वैयक्तिक तथा अविचलित भाव से कर्म करना सीखना होगा।
आर्य योद्धा का यही धर्म है। यह कहता है कि "ईश्वर को जान, अपने-आपको जान, मनुष्य की सहायता कर; धर्म की रक्षा कर, बिना भय, दुर्बलता और हिचकिचाहट के संसार में अपना युद्ध-कर्म कर। तू शाश्वत अविनाशी आत्मा है, तेरी आत्मा अमृतत्व के ऊर्ध्वगामी मार्ग पर चलती हुई इस संसार में आयी है; जीवन और मरण कुछ भी नहीं हैं, दुःख और क्लेश और कष्ट कुछ भी नहीं हैं, इन सबको जीतना और वश में करना होगा। अपने ही सुख, प्राप्ति और लाभ की ओर मत देख, अपितु ऊपर की ओर और चारों ओर देख, ऊपर उस प्रकाशमय शिखर को देख जिसकी ओर तू चढ़ रहा है, और अपने चारों ओर इस संग्राममय और संकटपूर्ण जगत् को देख जिसमें शुभ और अशुभ, उन्नति और अवनति परस्पर घोर संघर्ष में जकड़े हुए हैं। लोग तुझे सहायता के लिये पुकारते हैं, तू उनका लौह पुरुष है, लोकनायक है; तो सहायता कर, युद्ध कर। संहार कर यदि संहार के द्वारा ही जगत् की प्रगति हो, किन्तु जिसका संहार करे उससे घृणा न कर और न उन सब मरे हुए लोगों के लिये शोक ही कर। सर्वत्र उस एक ही आत्मा को जान, सब प्राणियों को अमर आत्माएँ समझ और शरीर को तो और कुछ नहीं बस मिट्टी समझ । अपना कर्म स्थिर, दृढ़ और सम भाव से कर, लड़ और शान से वीरगति को प्राप्त हो, या फिर पराक्रमी रूप से विजयी हो। क्योंकि भगवान् ने और तेरे स्वभाव ने तुझे यही काम पूरा करने के लिये दिया है।"
यहाँ हम देखते हैं कि आर्य पद्धति में किस प्रकार क्षत्रियों के अति उच्च आदर्श स्थापित किये जाते थे, और इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी उनके अपने-अपने उच्च आदर्श स्थापित किये जाते थे, उन्हें उन आदर्शों में ढाला जाता था ताकि निम्न प्रकृति किसी हद तक उन आदर्शों के अनुरूप वश में रहे। अपने शरीर के सुख-आराम के लिए जीना तो आर्य पद्धति के आदर्श में था ही नहीं।
परंतु प्रस्तुत प्रसंग में, जिन भिन्न-भिन्न आदशौं से व्यक्ति स्वयं को संचालित करता है वे एक दूसरे के अंतर्विरोध में आ खड़े हुए हैं, और भयानक बन गए हैं। ऐसे में जहाँ तक अपने कर्तव्य निर्वाह का प्रश्न उठता है, तो समझ नहीं आता कि गुरु के प्रति कर्त्तव्य, पितामह के प्रति कर्तव्य, अपने भाई-बंधुओं के प्रति कर्तव्य, या फिर अपने क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य में से कौनसे का निर्वाह किया जाए क्योंकि ये सभी कर्तव्य तो परस्पर विरोध में आ खड़े हुए हैं तथा किसी के भी निर्वाह करने से तो अवश्य ही कष्ट होने वाला है। और आखिर इस सबका परिणाम क्या होगा? यदि क्षत्रिय धर्म का पालन करे तो महाविनाश निश्चित है, सारी जाति ही नष्ट हो जाएगी और जो राज्य भोगने को मिलेगा वह खून से रंगा होगा। वहीं, यदि युद्ध न करे तो अधर्म की विजय होगी और यह तो उससे भी बुरी बात होगी। इसलिए इसमें से बचाव का कोई रास्ता ही नहीं है। और फिर इस आध्यात्मिक मनोभाव से भी, कि आत्मा अमर है और सभी में एक ही है, करना क्या चाहिये इसकी स्पष्टता नहीं होती। ऐसी स्थिति में कोई भी नैतिक युक्ति, या आदर्श या क्षत्रिय धर्म के पालन की युक्ति इसका कोई ऐसा उत्तर नहीं दे सकते जो कि उसकी आत्मा को संतुष्ट कर सके। क्योंकि यदि इसका समाधान इसी स्तर पर हो पाता तब तो गीता को और आगे विकसित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ व्यक्ति जीवन के मूल पर ही प्रश्न खड़ा कर देता है कि स्वयं इन नैतिक आधारों, मूल्यों में कोई न कोई मूलभूत त्रुटि है। इसीलिए गीता इस सारी समस्या को एक दूसरे ही स्तर पर ले जाकर इसका समाधान करती है जो कि निचले स्तर पर करना संभव नहीं है अन्यथा गीता के आगे के अध्यायों के निरूपण की आवश्यकता ही नहीं 8 hat pi साथ ही, श्रीअरविन्द का स्पर्श पाकर इन सारी ही समस्याओं का समाधान एक भव्य स्वरूप ग्रहण कर लेता है और इसी कारण श्रीमाताजी कहती हैं कि श्रीअरविन्द की टीका के कारण गीता का संदेश बिल्कुल निश्चयात्मक बन गया है और वह सारी मनुष्यजाति का उद्धार कर सकता है। श्रीअरविन्द तो इसे अतिमानस के छोर तक ले जाते हैं।
II. सांख्य और योग
अर्जुन की समस्याओं के इस प्रथम और संक्षिप्त उत्तर से (दूसरे उत्तर की ओर) मुड़ते क्षण तथा अपने प्रारंभिक शब्दों में ही जो एक आध्यात्मिक समाधान के प्रधान बिन्दु का संकेत करते हैं, श्रीगुरु एकाएक एक ऐसा भेद सांख्य और योग का भेद- प्रस्तुत कर देते हैं जो गीता को समझने हेतु चरम महत्त्व का है।
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु ।
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥
३९. हे पार्थी यह तुझे सांख्यशास्त्र के अनुसार बुद्धि (वस्तुओं का बुद्धियुक्त ज्ञान तथा इच्छाशक्ति) कही गयी है, अब तू योगविषयिणी इस बुद्धि को सुन, कारण इस बुद्धि के द्वारा योगयुक्त हो जाने पर तू कर्मों के बंधन को छोड़ देगा।
गीता के प्रथम छः अध्यायों का संपूर्ण उद्देश्य सांख्य और योग, इन दो प्रणालियों को, जिन्हें सामान्यतः एक-दूसरे से भिन्न और यहाँ तक कि विरोधी समझा जाता है, वेदांतिक सत्य की विशाल रूपरेखा में समन्वित करना है। सांख्य को ही आरंभबिंदु और आधार के रूप में लिया गया है; परंतु इसे आरंभ से ही, और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए बल अथवा प्रभाव के साथ योग के भावों और प्रणालियों से व्याप्त अथवा परिपूर्ण किया गया है और उसे योग के ही भाव में एक नया रूप दे दिया गया है। सांख्य और योग में जो वास्तविक भेद था, जिस प्रकार से प्रतीत होता है कि उस समय की धर्म-बुद्धि के समक्ष इसने अपने-आप को प्रस्तुत किया था, वह प्रथमतः यह था कि सांख्य अग्रसर हुआ ज्ञान के द्वारा तथा बुद्धियोग द्वारा जबकि योग अग्रसर हुआ कर्म द्वारा तथा क्रियाशील चेतना के रूपांतर के द्वारा। दूसरा भेद – जो प्रथम भेद का ही स्वाभाविक परिणाम 41 - 45 था कि, सांख्य पूर्ण निष्क्रियता और संन्यास की ओर ले जाने वाला माना जाता था जब कि योग को पर्याप्त रूप से कामना का आंतरिक त्याग, आत्मगत तत्त्वों का पवित्रीकरण माना जाता था जो कि कर्म की ओर और कर्मों को भगवान् की ओर मोड़ कर दिव्य अस्तित्व और मुक्ति की ओर ले जाता था। फिर भी दोनों का उद्देश्य एक समान ही था, जन्म और इस पार्थिव अस्तित्व का अतिक्रमण तथा मानव-आत्मा का परमात्मा के साथ ऐक्य। तो कम-से-कम सांख्य और योग के बीच यह भेद तो है जैसा कि गीता उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है।
गीता अपने मूल में एक वेदांतिक-ग्रंथ है; वेदांत के जो तीन सर्वमान्य प्रमाणग्रंथ हैं उनमें यह भी एक है।.. परन्तु फिर भी इसके वेदांतिक विचार सर्वत्र ही और पूर्ण रूप से सांख्य और योग की चिंतन पद्धति द्वारा रंगे हुए हैं, प्रभावित हैं और इस रंग या प्रभाव के कारण इसका दर्शन एक विशिष्ट समन्वयात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है।.....
तब फिर, गीता द्वारा कहे गये ये सांख्य और योग क्या हैं? ये अवश्य ही वे प्रणालियाँ नहीं हैं जो हमें इन नामों से यथाक्रम ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका और पतंजलि के योगसूत्रों में निरूपित हुई प्राप्त होती हैं। यह सांख्यकारिका का सांख्य नहीं 3 - 34 - 7 -कम सांख्य शब्द से जो सामान्य धारणा होती है, वह नहीं है; क्योंकि गीता कहीं भी क्षण भर के लिये भी सत्ता के मूल सत्य के रूप में पुरुषों की अनेकता को स्वीकार नहीं करती, अपितु सांख्य-परंपरा जिसका जोरदार शब्दों में इन्कार करती है उसी 'एक' को गीता दृढ़ता के साथ 'आत्मा' और 'पुरुष', फिर उसी 'एक' को 'परमेश्वर', 'ईश्वर' या 'पुरुषोत्तम' तथा 'ईश्वर' को जगत् का आदि कारण घोषित करती है। आधुनिक परिभाषा में कहें तो, परंपरागत सांख्य अनीश्वरवादी है, पर गीता का सांख्य जगत्-विषयक ईश्वरवादी, बहुदेववादी और अद्वैतवादी मतों को स्वीकार करता है और सूक्ष्मतया समन्वित करता है।
न ही यह योग पतंजलि की योग-प्रणाली ही है; क्योंकि वह (पतंजलि का योगदर्शन) तो राजयोग की केवल एक शुद्ध रूप से आत्मनिष्ठ प्रणाली है, एक आंतरिक अनुशासन है, जो सीमित, अनम्य रूप से निर्धारित, कठोर और शास्त्रीय अथवा वैज्ञानिक रीति से क्रमबद्ध है, जिसके द्वारा मन को उत्तरोत्तर स्थिर-निस्तब्ध कर के समाधि में पहुँचाया जाता है जिससे हम आत्म-अतिक्रमण के लौकिक और पारलौकिक, दोनों फल प्राप्त कर सकें; लौकिक, आत्मा के ज्ञान और शक्तियों के महान् विस्तार द्वारा और पारलौकिक, भगवान् के साथ गए पारंपरिक शब्दों के प्रयोग से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसी तरह से योग के विषय में है। पतंजलि का योग तो एक विशिष्ट पद्धति है जिससे मन को शुद्ध करने से उसके अंदर शक्तियाँ जागृत होती हैं, अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं और समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। योग का अर्थ तो है भगवान् के साथ युक्त होना। आजकल आम तौर पर योग का अर्थ हठयोग या पतंजलि के योग से ही लगाया जाता है, और वह भी बड़े ही सीमित रूप में। परन्तु गीता का योग तो बहुत विशाल एवं व्यापक है, जिसमें हजारों तरीकों से परमात्मा से एकत्व प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार, गीता का योग उस विशाल दृष्टिकोण से योग है और उसी लचीले दृष्टिकोण से इसका सांख्य है।
पर सांख्य के सत्य क्या हैं? इस दर्शन ने अपना यह नाम अपनी विश्लेषणात्मक पद्धति के कारण प्राप्त किया है। सांख्य हमारी सत्ता के तत्त्वों का विश्लेषण, गणना, विभाजन और विवेचनात्मक विन्यास है, जिनके संयोजनों तथा उन संयोजनों के परिणामों को ही मनुष्य की साधारण बुद्धि देख पाती है। सांख्य दर्शन ने समन्वय साधन की कोई चेष्टा नहीं की। इस दर्शन का मूलभूत सिद्धांत वस्तुतः द्वैतवादी है, ठीक वेदांतिक मतों का वह सापेक्षिक (relative) द्वैत नहीं जो वे अपने-आप को उस 'द्वैत' नाम से पुकारते हैं, अपितु एक परम निरपेक्ष और तीक्ष्ण अथवा सुस्पष्ट रीति का द्वैत है। क्योंकि यह अस्तित्व या सत्ता का वर्णन केवल एक मूल तत्त्व के द्वारा नहीं अपितु दो मूल तत्त्वों के द्वारा करता है जिनका संयोग ही इस जगत् का कारण है- एक है पुरुष जो अकर्ता (निष्क्रिय तत्त्व) है और दूसरी है प्रकृति जो कीं (सक्रिय तत्त्व) है। पुरुष आत्मा है, आत्मा शब्द के साधारण और प्रचलित अर्थ में नहीं, अपितु उस विशुद्ध सचेतन सत्ता (पुरुष) के अर्थ में जो अचल, अक्षर और स्वयं-प्रकाशमान है। प्रकृति है ऊर्जा और उसकी प्रक्रिया। पुरुष स्वयं कुछ नहीं करता, पर वह प्रकृति और उसकी प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करता है; प्रकृति जड़-यांत्रिक है परंतु पुरुष में प्रतिबिंबित होकर वह अपने कर्म में चेतना का रूप धारण कर लेती है और इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और संहार अर्थात् जन्म, जीवन और मरण, चेतना और अवचेतना, इन्द्रियगम्य ज्ञान और बुद्धिगम्य ज्ञान तथा अज्ञान, कर्म और अकर्म, सुख और दुःख, ये सब विषय उत्पन्न होते हैं और पुरुष प्रकृति के प्रभाव में आकर इन सबको अपने ऊपर आरोपित कर लेता है जबकि वास्तव में ये बिल्कुल भी उससे संबद्ध नहीं हैं अपितु एकमात्र प्रकृति की क्रिया अथवा उसकी गति से संबंधित हैं।
चूंकि प्रकृति तीन गुणों अर्थात् ऊर्जा की तीन मूलभूत अवस्थाओं से निर्मित है; सत्त्व, जो ज्ञान का मूल है, ऊर्जा की क्रियाओं की स्थिति बनाए रखता है; रजस्, जो शक्ति और कर्म का मूल है, ऊर्जा की क्रियाओं की सृष्टि करता है; तमस्, जो जड़ता और अज्ञान का मूल है, और जो सत्त्व और रजस् का निषेध या विपर्यय है, उस सबका संहार या विध्वंस करता है जिसकी वे सृष्टि करते तथा स्थिति रखते हैं। प्रकृति के ये तीन गुण जब साम्यावस्था में होते हैं तब सब कुछ ठहरा हुआ स्थिर पड़ा रहता है, कोई गति, कर्म या सृष्टि नहीं होती और इसलिए चेतन 'आत्मा' की अक्षर ज्योतिर्मयी सत्ता में आभासित या प्रतिबिंबित होनेवाली भी कोई वस्तु नहीं होती। परंतु जब इस साम्यावस्था में भंग होता है तब तीनों गुण विषमता की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसमें कि वे एक-दूसरे से संघर्ष करते और एक-दूसरे पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करते हैं, और उसी से विश्व को प्रकट करने वाला यह सृष्टि, स्थिति और संहार का विरामरहित व्यापार आरम्भ होता है। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक पुरुष अपने अन्दर इस वैषम्य को, जो उसके सनातन स्वभाव को ढक देता और उस पर प्रकृति' के स्वभाव को आरोपित करता है, प्रतिभासित होने देता है।
-----------------
• जगत् के क्रमविकास के मूल में प्रकृति अपने तीनों गुणों सहित पदार्थों के मूलतत्त्व के रूप में अव्यक्त अचेतन अवस्था में रहती है, जिसमें से क्रमशः ऊर्जा या जड़तत्त्व की पाँच मूलभूत अवस्थाओं का विकास होता है... प्राचीन शास्त्रानुसार पंचमहाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पर यह स्मरण रखना होगा कि ये आधुनिक विज्ञान के अर्थ में ईमें मूलतत्त्व नहीं हैं, अपितु ये भौतिक ऊर्जा की ऐसी अति सूक्ष्म अवस्थाएँ हैं जिनका विशुद्ध स्वरूप इस स्थूल जगत् में कहीं भी प्राप्य नहीं है। सभी पदार्थ इन्हीं पाँच सूक्ष्म अवस्थाओं या तत्त्वों के संयोगों से सृष्ट होते हैं। और फिर, इन पाँचों महाभूतों में से, प्रत्येक महाभूत ऊर्जा या जड़तत्त्व के पाँच सूक्ष्म लक्षणों में से किसी एक लक्षण (तन्मात्रा) का आधार होता है। ये पंचतन्मात्राएँ हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। इन्हीं के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों को विषयों का ज्ञान होता है। इस प्रकार मूल प्रकृति से उत्पन्न इन पंचमहाभूतों और उनकी इन पंचतन्मात्राओं से, जिनके द्वारा स्थूल का बोध होता है, उसका विकास होता है जिसे आधुनिक भाषा में विश्व-सत्ता का वस्तुनिष्ठ पक्ष कहते हैं।
तेरह तत्त्व और हैं जिनसे विश्व ऊर्जा का आत्मनिष्ठ पक्ष निर्मित होता है- बुद्धि या महत्, अहंकार, मनस् और उसकी दस इन्द्रियाँ (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ)। मन मूल इन्द्रिय है जो सभी बाह्य पदार्थों का बोध करता और उन पर प्रतिक्रिया करता है; क्योंकि इसमें अंतर्मुखी (अनुमान, निष्कर्ष, आकलन आदि आत्मपरक क्रिया) और बहिर्मुखी (स्नायुओं की संवेदनादि क्रिया) दोनों क्रियाएँ साथ-साथ होती रहती हैं: इन्द्रियानुभव के द्वारा यह उन विषयों को ग्रहण करता है जिन्हें गीता 'बाह्य स्पर्श' कहती है और उनके द्वारा जगत् के विषय में अपना विचार बनाता है और सक्रिय प्राणशक्ति द्वारा उस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ करता है। परन्तु पाँच ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध (पंच तन्मात्राएँ) जिनके विषय हैं यह अपनी ग्रहण करने की अति सामान्य क्रियाओं में विशिष्टता या समुन्नतता प्राप्त करता है (अर्थात् उन्हें भली भाँति चलाता है। इसी प्रकार पाँच कर्मेन्द्रियों की सहायता से वाणी, गति, वस्तुओं के ग्रहण, विसर्जन और प्रजनन के द्वारा यह प्रतिक्रिया करनेवाली प्राणी की कुछ अत्यावश्यक मूलभूत क्रियाओं को विशेष रूप से चलाता है। बुद्धि जो विवेक-तत्त्व है, वह साथ-ही-साथ बोध और संकल्प दोनों है, यह प्रकृति की वह शक्ति है जो विवेक के द्वारा पदार्थों में (उनके गुणधर्मानुसार) भेद करती है और समन्वय साधित करती है। अहंकार, अहं-बोध, बुद्धि में निहित आत्मपरक तत्त्व है जिससे पुरुष प्रकृति और उसकी क्रियाओं के साथ अपने-आप को तदात्म करने के लिए प्रेरित होता है। परन्तु ये आत्मनिष्ठ तत्त्व स्वयं उतने ही जड़, निश्चेतन प्रकृति के उतने हो अंश हैं जितने कि वे तत्त्व जो उसकी वस्तुनिष्ठ क्रियाओं का गठन करते हैं। यदि यह समझने में हम कठिनाई अनुभव करते हों कि किस प्रकार बुद्धि और मन जड़ निश्चेतन प्रकृति के ही गुण या लक्षण तथा स्वयं भी जड़ हो सकते हैं तो हमें इतना भर स्मरण रखना चाहिये कि स्वयं आधुनिक विज्ञान भी (अपने सभी विश्लेषणों के पश्चात्) इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है। यहाँ तक कि परमाणु की अचेतन जड़ क्रिया में भी एक शक्ति होती है जिसे निश्चेतन इच्छाशक्ति ही कह सकते हैं तथा प्रकृति के सभी कार्यों में यही व्यापक इच्छाशक्ति निश्चेतन रूप से बुद्धि के कार्य करती है। जिसे हम मानसिक बुद्धि कहते हैं वह तत्त्वतः ठीक वही चीज है जो इस जड़-भौतिक विश्व को सभी क्रियाओं में अवचेतन रूप से विवेक (गुणधर्मानुसार भेद) करने और समन्वित करने का काम करती है, और आधुनिक विज्ञान यह दिखलाने का यत्न करता है कि स्वयं सचेतन मन भी निश्चेतन प्रकृति को जड़ क्रिया का ही परिणाम और प्रतिलिपि है। परन्तु आधुनिक विज्ञान जिस विषय को अँधेरे में छोड़ देता है अर्थात् किस प्रकार जड़ और निश्चेतन सचेतन का रूप धारण करता है, सांख्यशास्त्र उसको भी व्याख्या कर देता है।
सारी प्रकृति वस्तुतः आत्मगत (subjective) अर्थात् चेतना-संबंधी है। यह आत्मगत दृष्टि से ही विकसित होती है। क्योंकि दो तरह के विभाजन हैं - एक है मूल प्रकृति और दूसरा है पुरुष, अर्थात् एक तो है मूल तत्त्व जिसका साक्षित्व किया जाता है और दूसरा है साक्षी तत्त्व या द्रष्टा जो उसे देखता है। इन दोनों के बिना सृष्टि हो ही नहीं सकती। यदि ऐसी कोई सृष्टि है जिसका कभी किसी ने साक्षित्व या अवलोकन न किया हो तो उसके अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं है। और यदि साक्षी पक्ष तो है पर कोई सृष्टि नहीं तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। सृष्टि होने के लिए दोनों का समामेलन आवश्यक है। सृष्टि की जो यह सारी प्रतीति या प्रकटन है वह मूल प्रकृति से आरम्भ होता है। मूल प्रकृति के अन्दर परमात्मा की सारी संभावनाएँ निहित हैं। वर्तमान सृष्टि का सारा प्रयास एकमेवाद्वितीय के सूत्र को - जो कि सभी कुछ के मूल में अंतर्निहित है - बहुलता में प्रकट करना है। इस बहुलता को प्रकट करने के लिए जब तक पृथक्ता का भान न हो तब तक बहुलता का बोध नहीं होता। इसलिए इसमें 'अहं' सबसे पहले आता है - पुरुष, मूल प्रकृति और अहंकार। अहंकार आने के बाद समस्या यह आती है कि व्यक्ति दूसरों के साथ, अर्थात् जो निज-सत्ता से पृथक् हैं उनके साथ किस प्रकार क्रिया-व्यापार करे क्योंकि जब व्यक्ति एकमेव ही रहता है तब तक तब स्वयं और दूसरे जैसा कोई भेद ही नहीं होता, परन्तु पृथक्ता के बोध के साथ परस्पर क्रिया-व्यापार का बोध भी आता है। इसके लिए फिर आती है 'बुद्धि' - विवेक या भेद दृष्टि - जो यह पता लगाती है कि क्या करना चाहिये और कैसे करना चाहिये। यदि 'अहंकार' होगा तो वह 'बुद्धि' को प्रक्षिप्त करेगा। 'अहंकार' मूल प्रकृति से प्रक्षिप्त होता है। अब जब बुद्धि इस परिदृश्य में शामिल हो जाती है तो उसे निरंतर सूचना की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर वह सही-गलत, उचित-अनुचित का निर्णय कर सके, और जब उसे सूचना के घटकों का पता चल जाए तब यह निर्णय करे सके कि उनके साथ कैसा व्यवहार करे। इस हेतु के लिए बुद्धि अपने-आप को प्रक्षिप्त करती है मनस् के रूप में। वस्तुतः मनस् ही एक मौलिक इंद्रिय है बाकी तो सब भौतिक जड़ सृष्टि है। मनस् में यह क्षमता होती है कि वह देश-काल की सीमा से परे भी जान सकता है, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जान सकता है और वह देश से भी सीमित नहीं होता, वह कितनी भी दूरी की चीजों को जान सकता है। ये सारी क्षमताएँ मनस् में निहित हैं। यदि मानव मनस् की ये सारी क्षमताएँ काम में लेते तो सारी सृष्टि बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती और जैसा भौतिक निर्माण हमें गोचर होता है वैसा कदाचित् ही हमें दिखाई देता क्योंकि मनस् में तो देश और काल की सीमाएँ भी लचीली होती हैं। परंतु इस सृष्टि को बनाने के लिए मनस् के पंख काट दिये गये, या यों कहें कि उन्हें कुछ हद तक बाँध दिया गया। इसलिए किन्हीं मनुष्यों में वह अपनी क्षमताओं को अधिक काम में लेता है जबकि दूसरों में अपनी क्षमताओं को उतना काम में नहीं लेता। उदाहरण के लिए समान ही दृश्य को देखकर भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं क्योंकि उनमें मनस् की योग्यता में अन्तर होता है। भले ही उन सब में इन्द्रियाँ तो लगभग समान ही सूचना दे रही होती हैं परन्तु वह सूचना जाती है मनस् के पास जो कि उस अनुपात में और उस तरीके से उन सूचनाओं की भिन्न-भिन्न व्याख्या करता है जैसी उसकी भिन्न-भिन्न क्षमताएँ या शक्ति-सामर्थ्य होते हैं। उदाहरण के लिए एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा एक कलाकार की क्षमताएँ अधिक विकसित होती हैं इसलिए वह इंद्रियों से मिली सूचना के आधार पर सामान्य मनुष्य से सर्वथा भिन्न तरीके से निष्कर्ष निकालता है। इस प्रकार मनस् एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। वास्तव में तो केवल मनस् ही एकमात्र इंद्रिय है बाकी तो सब उसके अधीनस्थ सहायक हैं। परंतु इंद्रियों के कारण मनस् की क्षमताओं पर तथा उसकी क्रिया पर अंकुश लग जाता है। इन इंद्रियों की सहायता से वह कुछ चीजें तो स्पष्ट रूप से जान लेता है परंतु अधिकांश चीजों में ये इंद्रियाँ उसकी सहज शक्ति को सीमित कर देती हैं। ये उसे इस रूप में सीमित कर देती हैं कि स्वयं अपने-आप में पर्याप्त होते हुए भी वह अपने-आप को पाँच ज्ञानेंद्रियों और पाँच कर्मेन्द्रियों में प्रक्षिप्त करता है और उनकी सहायता से क्रिया करता है। ज्ञानेन्द्रियाँ बुद्धि को सूचना देती हैं। बुद्धि निर्णय करती है और साथ ही अपना स्वयं का मंतव्य भी जोड़ती है और तब जो कुछ करना है उस बारे में सूचना कर्मेन्द्रियों तक पहुँचा दी जाती है। इस प्रकार मनस् ने पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पाँच कर्मेन्द्रियों में अपना पसारा कर रखा है। अब, ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए तन्मात्राओं की आवश्यकता होती है। आँखों को दृष्टि की, कानों को श्रवण शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये पाँच तन्मात्राएँ हैं। इन पाँच तन्मात्राओं के माध्यम से इन्द्रियाँ जानने का प्रयास करती हैं। ये पाँच तन्मात्राएँ पंच महाभूतों को जन्म देती हैं। वास्तव में, अपने-आप में कोई जड़-तत्त्व नहीं है परंतु जो कुछ भी है उसे ये तन्मात्राएँ अपने अनुसार परिवर्तित कर के पाँच महाभूतों के रूप में प्रकट करती हैं। इसीलिए श्रीअरविन्द कहते हैं कि विज्ञान जितना ही अधिक आगे जाएगा उतना ही उसे यह पता लग जाएगा कि जड़-तत्त्व जैसी कोई चीज है ही नहीं, और यही बात तो हमारा सांख्य-शास्त्र पहले ही घोषित कर चुका है। सभी कुछ केवल ऊर्जा ही है। ये तन्मात्राएँ भी एक सूक्ष्म ऊर्जा का रूप हैं जो कि पंचमहाभूतों के दिखावे को प्रकट करती हैं। इन पंच महाभूतों का बोध इंद्रियाँ पंच तन्मात्राओं के माध्यम से करती हैं। इन्द्रियाँ मनस् का ही विस्तार, उसी का प्रक्षेपण हैं। मनस् इनकी सूचना को बुद्धि के पास भेजता है जिसका कि विवेक-बुद्धि विश्लेषण करती है। परंतु इसमें समस्या यह है कि हमारा क्रियाशील मन क्रिया-प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत उतावला रहता है जिससे प्रायः बुद्धि को विवेक के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। बुद्धि के कार्य करने से पहले ही वह हस्तक्षेप कर बैठता है। इन्द्रियों से मिली सूचनाओं पर वह बीच में ही तुरंत क्रिया करना आरम्भ कर देता है। बिना सोचे-विचारे ही वह लड़ाई-झगड़े में, गाली-गलौच तक में संलग्न हो जाता है। इसीलिए श्रीमाताजी कहती हैं कि थोड़ा पीछे हटो, और विवेकपूर्वक विचार करो और तब कार्य करो। यदि हम पीछे हटकर कुछ विचार करेंगे तो बुद्धि को हस्तक्षेप करने का कुछ मौका मिलेगा और इससे फिर एक हद से अधिक मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया पर कुछ अंकुश लग जाएगा। और ज्यों ही बुद्धि से विवेक आएगा, वह व्यक्ति की कर्मेन्द्रियों को काम में लेगा। उस विवेक की अभिव्यक्ति के लिए जिस किसी भी कर्मेन्द्रिय की आवश्यकता होगी वैसी काम में ले ली जाएगी - जैसे कि वाणी की आवश्यकता होगी तो बोल कर क्रिया होगी, हाथों से क्रिया की आवश्यकता होगी तो तदनुरूप क्रिया होगी। इस तरह से सृष्टि का यह सारा ही व्यापार चालू हो जाता है। हमारे लगभग सभी शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि जहाँ तक सृष्टि की प्रतीति की व्याख्या की बात है, इसके तत्त्वों के परिगणन की बात है, तो सांख्य का वर्णन लगभग सही है। तो इस प्रकार ये चौबीस तत्त्व हुए और पच्चीसवाँ तत्त्व है अवलोकन करने वाला साक्षी तत्त्व। यदि वह न हो तो किसी चीज का कोई अर्थ ही न होगा, उसके अवलोकन से ही सारी सृष्टि का अर्थ है।
अपनी एकमेव की चेतना के अंदर यह अहंकार या फिर पृथक्ता का बोध तब आएगा जब मूल प्रकृति के अंदर कोई क्षोभ उत्पन्न होगा। यदि वह साम्यावस्था में ही रहे, तो पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही होंगे और इस कारण सृष्टि-क्रम नहीं होगा। परन्तु उसमें यदि क्षोभ होगा तो उनमें विच्छेद उत्पन्न हो जाएगा। साम्यावस्था में तीन गुणों का क्षोभ प्रकट नहीं होता। अहंकार भी तीन प्रकार का है - सात्त्विक, राजसिक, तामसिक । यदि ये तीनों नहीं होंगे तो अहंकार रहेगा ही नहीं, सृष्टि का निर्माण ही नहीं होगा। अब चूँकि जड़-तत्त्व जैसी कोई चीज नहीं है और सब कुछ केवल आत्मपरक चेतना के अनुसार दिखाई देता है इसीलिये इसे 'लोक' कहते हैं, अर्थात् अवलोकनकारी चेतना के अनुसार ही प्रतीति होती है। यदि इन्द्रियों की संरचना दूसरे ही तरीके की होगी तो हमें बिल्कुल भिन्न प्रतीति होगी। इसीलिए यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सूक्ष्म जगतों में हम पाएँगे कि वहाँ चीजें बहुत अधिक सुन्दर हैं, क्योंकि यहाँ भौतिक स्तर तक आते-आते बहुत प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है और उनका उतना सौंदर्य अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। वहाँ वे अपने अधिक सच्चे रूप में विद्यमान हैं। इसलिए जो यहाँ भद्दा दिखाई देता है उसी का रूप वहाँ बहुत सुन्दर है, और जो कुछ यहाँ सुन्दर दिखाई देता है उसका मूल रूप तो वहाँ दिव्य है, अपूर्व है। अतः ये सभी 'लोक' हैं अर्थात् जिस चेतना के स्तर से हम देखते हैं ये वैसे ही दिखाई देते हैं। सारे लोकों में ही पुरुष और प्रकृति का खेल है। जिस तरह की हमारी इन्द्रियाँ होंगी उसी तरीके का हमें अनुभव होगा। और वास्तव में तो क्या है या क्या नहीं इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आखिर परमात्मा को जाना ही कैसे जा सकता है। यह तो हमारा केवल देखने का एक तरीका-मात्र है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारी चेतना कैसी है। वह जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार के जगत् का अनुभव हमें होगा। पशुओं में भी कुछ को मनुष्यों से अधिक रंग दिखाई देते हैं, कुछ को रंग दिखते ही नहीं। मनुष्यों की अपेक्षा कुत्तों में घ्राण-शक्ति बहुत अधिक विकसित होती है। इस प्रकार इन्द्रियों के विकास का कोई अन्त नहीं है। अतः जगत् हमें किस रूप में दिखाई देगा यह इस पर निर्भर करेगा कि इंद्रियों ने अपना केंद्र किस चेतना पर स्थापित कर रखा है। ये सारा जगत् एक 'लोक' है, परमात्मा को देखने का एक तरीका है। चूंकि अपने-आप में उस एक ही सद्वस्तु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है अतः कसी निश्चित स्तर से देखने पर ही जड़-तत्त्व नजर आता है, अन्यथा नहीं। बहुत-सी ऐसी सृष्टियाँ हैं जिन्हें जड़-तत्त्व का आभास तक नहीं है। भौतिक जगत् में हमें बीच में रिक्तता या शून्यता नजर आती है, परंतु श्रीमाँ कहती हैं कि कहीं कोई रिक्तता है ही नहीं, सभी कुछ में प्रचुर रूप से सृष्टि भरी हुई है, बस केवल हमारी चेतना को, हमारी इंद्रियों को वह गोचर नहीं होता।
श्रीअरविन्द यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि गीता ने सांख्य को किस प्रकार अपनाया है जिससे कि हम उसे एक उचित परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं और किसी अनावश्यक भ्रांति से बच सकते हैं।
परंतु जब वह अपनी इस अनुमति को हटा लेता है तब तीनों गुण फिर साम्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और पुरुष अपने सनातन अविकार्य अचल स्वरूप में लौट आता है; वह विश्व-प्रपंच से मुक्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि अपने अन्दर प्रकृति को आभासित होने देना और यह अनुमति देना या लौटा लेना ही पुरुष के एकमात्र अधिकार हैं; प्रकृति को अपने अन्दर आभासित देखने के नाते पुरुष गीता की भाषा में साक्षी और अनुमति देने के नाते अनुमंता है, परंतु सक्रिय या प्रभावी रूप से ईश्वर नहीं है। यहाँ तक कि उसका अनुमति देना भी निष्क्रिय है। कर्ममात्र ही, चाहे वह आत्मनिष्ठ हो या वस्तुनिष्ठ, आत्मा का स्वधर्म नहीं, उसके लिए विजातीय है, उसमें न कोई सक्रिय संकल्प है न कोई सक्रिय बुद्धि अथवा ज्ञान...
सांख्य के अनुसार यह बुद्धि और संकल्प सर्वथा प्रकृति की यांत्रिक ऊर्जा के अंग हैं, पुरुष के गुणधर्म नहीं हैं; ये दोनों ही बुद्धि-तत्त्व हैं जो कि जगत् के चौबीस तत्त्वों में से एक तत्त्व है।... बुद्धि जो विवेक तत्त्व है, वह एक ही साथ बोध और संकल्प दोनों है, यह प्रकृति की वह शक्ति है जो विवेक के द्वारा पदार्थों को उनके गुणधर्मानुसार पृथक् करती और उनमें संगति बैठाती है। अहंकार बुद्धि का आत्मगत या अहंगत वह तत्त्व है जिससे पुरुष प्रकृति और उसकी क्रियाओं के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है।...
अवश्य ही हमारे इस जगत् में बहुत-सी चीजें हैं जिन्हें सांख्यशास्त्र बिल्कुल भी निरूपित नहीं करता और करता भी है तो संतोषप्रद रूप से नहीं, परन्तु यदि हमें उसके तत्त्वों में वैश्विक प्रक्रियाओं की केवल एक बौद्धिक या तर्कसंगत व्याख्या ही चाहिए जो कि सभी प्राचीन दर्शनों के समान ही लक्ष्य - लक्ष्य है विश्व-प्रकृति से ग्रसित आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर होने में एक आधार के रूप में हो, तब तो सांख्य का जगत्-निरूपण और मुक्ति का मार्ग उतना ही उत्तम और प्रभाषकारी है जितना कि अन्य कोई मार्ग। यहाँ जो बात पहले समझ में नहीं आती वह यह है कि सांख्यदर्शन प्रकृति को एक, और पुरुष को अनेक बताकर अपने द्वैत सिद्धांत में बहुत्व के तत्त्व का प्रवेश क्यों कराता है।... परन्तु पदार्थों के मूल तत्त्वों के निरीक्षण की कठोर विश्लेषण-पद्धति के फलस्वरूप पुरुष-बहुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करना सांख्य के लिये अनिवार्य था।... विश्व और उसकी प्रक्रिया को एक पुरुष और एक प्रकृति के व्यापार के रूप में समझाया जा सकता है, किन्तु इससे विश्व में सचेतन जीवों की बहुलता का समाधान नहीं होता।
फिर इतनी ही विकट एक और कठिनाई है। अन्य दर्शनों की ही तरह सांख्य ने भी 'मोक्ष' को अपना लक्ष्य रखा है। यह मोक्ष... पुरुष द्वारा प्रकृति के कर्मों से अपनी अनुमति हटा लेने से प्राप्त होता है... तब अवश्य ही उसके गुणों को साम्यावस्था में आना ही होगा, विश्व-प्रपंच अवश्य ही बंद हो जाएगा और पुरुष को अपनी अचल शांति में लौट जाना होगा। परन्तु यदि पुरुष एक ही होता और विवेक तत्त्व (बुद्धि और संकल्प) अपने भ्रम से निवृत्त हो जाता तो सारा विश्व-प्रपंच ही बन्द हो जाता। परंतु जैसा यह है, इसमें हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। असंख्य प्राणियों में से कुछ ही मोक्ष को प्राप्त होते या इसकी ओर अग्रसर होते हैं; शेष सब इससे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होते, और न ही विश्व प्रकृति की जो क्रीड़ा उनके साथ हो रही है उसमें इस छोटे-मोटे त्याग से रत्ती भर भी असुविधा ही होती है जब कि उसकी सारी प्रक्रियाओं का ही अंत हो जाना चाहिये था। केवल अनेक स्वतंत्र पुरुषों के सिद्धांत द्वारा ही इस तथ्य की व्याख्या की जा सकती है। वेदांतिक अद्वैतवाद के दृष्टिकोण से यदि इसकी कोई न्याय-संगत व्याख्या हो सकती है तो वह है मायावाद। परंतु मायावाद को मान लेने पर तो यह सारा प्रपंच एक स्वप्नमात्र हो जाता है, तब बंधन और मुक्ति दोनों ही अवास्तविकता (अथवा माया) की अवस्थाएँ, माया की अनुभवजन्य भ्रांतिमात्र हो जाती हैं; वास्तविकता में न कोई मुक्त है, न कोई बद्ध। वस्तुओं का अधिक यथार्थवादी सांख्य दृष्टिकोण सृष्टि-विषयक इस भ्रांतिजनक विचार को स्वीकार नहीं करता (कि यह सब दृष्टिभ्रम है) और इसलिए वह वेदांत के इस समाधान को ग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार यहाँ भी हम देखेंगे कि जगत् के सांख्य विश्लेषण से प्राप्त तथ्यों का बहु पुरुष का सिद्धांत एक अपरिहार्य निष्कर्ष है।
गीता सांख्य के इस विश्लेषण से आरंभ करती है और जहाँ वह योग का निरूपण कर रही होती है वहाँ भी पहले तो सांख्य के इस विचार को ही लगभग पूर्णतया स्वीकार करती प्रतीत होती है। वह प्रकृति, उसके तीन गुणों और चौबीस तत्त्वों को स्वीकार करती है; प्रकृति पर समस्त कर्मों के आरोपण को और पुरुष के अकर्तापन को भी गीता स्वीकार करती है; विश्व में सचेतन प्राणियों की बहुलता होने को भी स्वीकार करती है, तादात्म्यकारी अहं-भाव के तथा बुद्धि की भेदभाव करनेवाली क्रिया के लय को और प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया के अतिक्रमण को मोक्ष के साधन के रूप में स्वीकार करती है। आरंभ से ही अर्जुन से जिस योग की साधना करने को कहा जा रहा है, वह बुद्धि द्वारा योग है। परन्तु इसमें एक महत्त्वपूर्ण भिन्नता या भेद है, - यहाँ पुरुष को एक माना गया है, अनेक नहीं।... इससे वह बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है जिसको सांख्य का बहुपुरुषवाद टाल जाता है, और किसी सर्वथा नये समाधान की आवश्यकता खड़ी हो जाती है। गीता यह समाधान, अपने वेदांतिक सांख्य में वेदांतिक योग के सिद्धांतों और तत्त्वों को लाकर करती है।
जो पहला महत्त्वपूर्ण नया सिद्धांत हमें देखने को मिलता है वह स्वयं पुरुषसंबंधी धारणा में है।... कठोर सांख्य-विश्लेषण में... 'पुरुष' साक्षी है, अनुमति का स्रोत है, आभास या प्रतिबिंबन के द्वारा प्रकृति के कर्म को धारण करनेवाला है, - साक्षी, अनुमंता और भर्ता है, इसके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं। परन्तु गीता-प्रतिपादित पुरुष प्रकृति का प्रभु भी है, वह ईश्वर है।... जहाँ 'संकल्पात्मक' बुद्धि की क्रिया प्रकृति की क्रिया है (के हाथ में है), वहाँ बुद्धि को आधार और प्रकाश पुरुष द्वारा सक्रिय रूप से प्रदान किये जाते हैं, वह केवल साक्षी ही नहीं, अपितु ज्ञाता और ईश्वर भी है, ज्ञान और संकल्प का स्वामी भी है। प्रकृति की कर्म में प्रवृत्ति का वही परम कारण है और वही उसकी कर्म से निवृत्ति का भी परम कारण है। सांख्य-विश्लेषण में पुरुष और प्रकृति अपने द्वैत भाव में विश्व (उत्पत्ति) के कारण हैं; और इस समन्वयात्मक सांख्य में पुरुष, अपनी प्रकृति के द्वारा, विश्व का एकमात्र कारण है। एकाएक हम देख सकते हैं कि सांख्य की कठोर अतिविशुद्धतावादी या कट्टरपंथी पारंपरिक विश्लेषण-प्रणाली से हम कितनी दूर निकल आये हैं...
तो फिर विश्व में जो अनेक सचेतन प्राणी हैं, उनका क्या? वे तो ईश नहीं प्रतीत होते, उल्टे बहुत हद तक अनीश ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये त्रिगुण की क्रिया और अहं-भाव की भ्रांति के अधीन हैं, और यदि ये सब एक ही आत्मा हैं, जैसा कि गीता का आशय प्रतीत होता है, तो यह प्रकृति में लीनता, वश्यता और भ्रांति कहाँ से उत्पन्न हो गई, अथवा इसका सिवाय यह कहने के कि पुरुष सर्वथा निष्क्रिय है, दूसरा क्या समाधान है? और, फिर पुरुष का यह बहुत्व कहाँ से आया? अथवा यह क्या बात है कि जहाँ उस एक, अद्वितीय पुरुष की किसी एक शरीर और मन में तो मुक्ति होती है, वहीं अन्य शरीरों और मनों में वह बंधन के भ्रम में बना रहता है? ये ऐसी शंकाएँ हैं जिनका समाधान किये बिना यों ही आगे नहीं जाया जा सकता।
गीता अपने बाद के अध्यायों में इन सब शंकाओं का प्रकृति और पुरुष के एक विश्लेषण द्वारा उत्तर देती है, जो विश्लेषण कुछ ऐसे नवीन तत्त्वों को सम्मिलित कर लेता है जो एक वेदांतिक योग के लिए तो बिल्कुल संगत हो हैं किन्तु परंपरागत सांख्य के लिये विजातीय हैं। यह तीन पुरुषों या यों कहें एक पुरुष की तीन अवस्थाओं का उल्लेख करती है.... क्षर, अक्षर और उत्तम। क्षर है प्रकृति, 'स्वभाव', जो गतिशील, परिवर्तनशील (क्षरणशील) है, यह जीव (आत्मा) की बहुविध अभिव्यक्ति या रूप धारण करना है, यहाँ पर जो पुरुष है वह दिव्य सत्ता (पुरुष) की बहुरूपता या विविधता है; यही बहुपुरुष है, यह पुरुष प्रकृति से स्वतंत्र नहीं है, अपितु यह 'प्रकृतिस्थ पुरुष' है। अक्षर, कूटस्थ, अविकार्य पुरुष निश्चल-नीरव और निष्क्रिय आत्मा है, यह दिव्य सत्ता (पुरुष) की एकरूपता या एकत्वावस्था है, यहाँ पुरुष प्रकृति का साक्षी है, पर प्रकृति के कार्यों में लिप्त नहीं; यह प्रकृति और उसके कर्मों से मुक्त, अकर्ता पुरुष है। उत्तम पुरुष परमेश्वर, परंब्रह्म, परमात्मा है, जिसमें अक्षर का एकत्व और क्षर का बहुत्व, दोनों ही अवस्थाएँ सन्निविष्ट हैं। वह अपनी प्रकृति की विशाल गतिशीलता और कर्म के द्वारा, अपनी (कर्ती) शक्ति, अपने संकल्प और सामर्थ्य के द्वारा जगत् में अपने-आपको व्यक्त करता है, और अपनी सत्ता की महत्तर निस्तब्धता और अचलता के द्वारा उससे अलग रहता है; फिर भी वह अपने पुरुषोत्तम-रूप में, प्रकृति से अलगाव और प्रकृति से आसक्ति, इन दोनों अवस्थाओं के ही परे है। पुरुषोत्तम की यह धारणा यद्यपि उपनिषदों में निरंतर ही अभिप्रेत है, तथापि इसे अलग कर के सुस्पष्ट और सुनिश्चित रूप से गीता द्वारा ही सामने रखा गया है और इसने भारतीय धार्मिक चेतना के उत्तरवर्ती नए विकासों पर बड़ा भारी प्रभाव डाला है। अद्वैतवाद की कठोर सूत्रबद्ध परिभाषाओं का अतिक्रम कर जाने का दावा करने वाले उच्चतम भक्तियोग का आधार यही पुरुषोत्तमसंबंधी धारणा है और भक्ति-प्रधान पुराणों के पीछे भी यही है।
यदि अनेक पुरुष नहीं होंगे और केवल एक ही पुरुष होगा तो उसके लय के साथ ही सारी सृष्टि का भी अंत हो जाएगा। अतः, गीता कहती कि पुरुष तो एक ही है परन्तु उसकी तीन अवस्थाएँ होती हैं। हमें जो बहुत्व गोचर होता है वह तो अहं के कारण है, वास्तव में बहुत्व नहीं है। सारे जगत् के निर्माण में पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही हैं, वे केवल रूप दो धारण करते हैं। इसमें जिसे हम पुरुष या ईश्वर पक्ष कहते हैं वह सब कुछ का संचालन करता है। और जो प्रकृति पक्ष है वह उस पुरुष की प्रसन्नता के निमित्त ही सब कुछ करता है। वही सभी कुछ का निर्माता है। पुरुषोत्तम ही सभी कुछ का नियंता है। इसलिए जब किसी प्रकृति के साथ तादात्म्य के अंदर वह एक केंद्र (क्षर-भाव) से हटकर अक्षर की निर्लिप्त अवस्था अपना लेता है तब वह उसमें निवास करने लगता है, और ऐसा करने से अन्य किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्य सभी अपने उसी क्षर भाव में चलते रहेंगे। क्योंकि यह सब सृष्टि या निर्माण कोई अकस्मात् संयोग के द्वारा नहीं हुआ, यह तो पुरुष की सोची-समझी क्रिया है। वह स्वयं तो ईश्वर है, इसलिए उसके द्वारा एक अहंकारमय चेतना के अंदर अपना क्षर से भाव बदलकर अक्षर अपना लेने से उसकी यह सोची-समझी क्रिया क्यों प्रभावित होगी? किसी एक अहं चेतना में वह क्षर से मुक्त होकर अक्षर भाव में निवास करने लगेगा, क्योंकि पुरुषोत्तम तो सदा ही क्षर और अक्षर दोनों ही है और उनसे परे भी है। इसलिए इस पद्धति में अनेक पुरुषों की आवश्यकता नहीं रहती। और फिर, शंकराचार्य आदि का एक अन्य मत भी है जिसके अनुसार केवल दो ही भाव हैं - क्षर और अक्षर। या तो व्यक्ति क्षर भाव में लिप्त रहता है, या फिर उससे मुक्त होकर अक्षर भाव में चला जाता है, और तब प्रकृति शांत हो जाती है और तब कोई प्रपंच नहीं रहता। परंतु इसमें भक्ति की तो कोई संभावना ही नहीं रहती। आखिर अक्षर भाव में व्यक्ति किसकी भक्ति करेगा? इसलिए जब हम पुरुषोत्तम की बात करते हैं तो उनकी भक्ति की जा सकती है जो सारी सृष्टि के नियामक हैं, सब कुछ को उत्पन्न करने वाले हैं। तब भक्तियोग संभव होता है। गीता भी इस तत्त्व को निर्णायक रूप से पन्द्रहवें अध्याय में प्रतिपादित करती है, उससे पहले तो वह 'अहम्', 'माम्' आदि पदों का प्रयोग करती है। पहले के अध्यायों में भगवान् यह कहते अवश्य हैं कि 'मैं यह हूँ' या फिर 'मेरे निमित्त कार्य करो' आदि-आदिः परंतु इस बात का बौद्धिक प्रतिपादन तो वे पन्द्रहवें अध्याय में ही करते हैं कि उनका सत्स्वरूप क्या है, वे वास्तव में कौन हैं, और यह कि वे क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं। और उन्हीं के प्रति भक्ति को अर्पित करना होगा। गीता के इसी प्रकार के पुरुषोत्तम तत्त्व के प्रतिपादन के कारण ही पुराणों आदि में भक्ति की इतनी संभावना बनती है। सांख्य में तो भक्ति की कोई संभावना नहीं है, अद्वैतवाद में भी क्षर और अक्षर दो ही पुरुषों को माना गया है, इसलिये उसमें भी भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। परंतु यहाँ श्रीकृष्ण अवतार के रूप में कहते हैं कि 'मैं पुरुषोत्तम हूँ। मैं क्षर-अक्षर दोनों से परे हूँ। सब कुछ मेरी इच्छा से ही होता है।' इसलिए उनके प्रति भक्ति और एकत्व प्राप्त करना उद्देश्य हो सकता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम तत्त्व के प्रतिपादन से गीता इस समस्या का समाधान करती है। प्रकृति को भी यह दो प्रकार की मानती है। यह जो गोचर हो रही है वह अपरा प्रकृति है, जो कि त्रिगुणमयी है, जबकि एक उच्चतर, परा प्रकृति भी है जो इस अपरा से परे है – 'परा प्रकृतिर्जीवभूता', जो कि जीव के रूप में भी प्रकट होती है, वह भगवान् की परा प्रकृति है। और जब भगवान् अवतार ग्रहण करते हैं, तब वे अपनी परा प्रकृति को अधीन करके जन्म ग्रहण करते हैं। वे इस अपरा प्रकृति के अधीन नहीं हैं। उन्हें अपने कार्य के लिए इसका जितना अंश आवश्यक होता है उतने अंश को वे स्वीकार करके धारण करते हैं बाकी को नहीं।
इस प्रकार इन सभी चीजों का स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि गीता के सांख्य और योग आम तौर पर इन नामों से जो समझे जाते हैं उनसे भिन्न हैं। इन चीजों को स्पष्टतः समझ लेना चाहिए ताकि कोई अयौक्तिक, परस्पर विरोधी तरीके की अदार्शनिक बातें न हों। वास्तव में देखा जाए तो, केवल परा प्रकृति ही कार्य करती है, अपरा प्रकृति तो कुछ है ही नहीं, वह तो केवल ऊपरी दिखावा-मात्र है वैसे ही जैसे कि परम् प्रभु ही सब कुछ करते हैं और उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं परंतु फिर भी हमारी चेतना पर इन्द्रियों और मन की बेड़ियों के कारण हमें ऐसा जगत् दिखाई देता है। जैसी हमारी चेतना होती है, वैसा ही जगत् हमें दिखाई देता है।
प्रश्न : सांख्य का जो वर्णन है वह क्या अपरा प्रकृति को लेकर ही है?
उत्तर : सांख्य परा या अपरा प्रकृति को नहीं मानता। वह तो एक ही प्रकृति को मानता है, जिसमें पुरुष है और बाकी उसकी विषय-वस्तु है जिसका वह साक्षित्व करता है। उसके अनुसार ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। बौद्ध धर्म भी यही कहता है कि इस गोचर प्रकृति को मिटा दो तो सब शून्य ही रह जाता है। वह तो पुरुष को भी नहीं मानता, उसे भी वह तो केवल प्रतीति या भ्रम ही बताता है, बाकी तो सब शून्य ही है। परंतु, ये सभी तो भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुभव हैं, और इन्हें ही संपूर्ण नहीं मान बैठना चाहिये। श्रीअरविन्द अपने पत्रों में इसकी पुष्टि करते हैं कि उन्हें स्वयं ये सभी और इनके अतिरिक्त भी अन्य उच्च अनुभव प्राप्त हुए, इसलिए उस समग्र सत्य को वे इन आंशिक अनुभवों से कैसे सीमित कर सकते हैं। गीता के इसी समन्वयात्मक स्वरूप के कारण श्रीअरविन्द ने इसे इतना महत्त्वपूर्ण मानकर इस पर अपनी टीका लिखी है। इसी कारण उन्होंने वेद और उपनिषदों पर अपनी टीका लिखी है। उनका अनुभव अतिशय रूप से विशाल था। और सच कहें तो, वेद, उपनिषद् और गीता आदि में क्या तत्त्व निहित है या उनका अपने-आप में क्या महत्त्व है, यह तो हम नहीं जानते परंतु हमारे अपने लिये इनका महत्त्व श्रीअरविन्द की दृष्टि से इनकी झाँकी प्राप्त करने के कारण, उन्हीं के शब्दों से इनमें जो प्राण का संचार हुआ है उसका रसास्वादन कर पाने के कारण है।
गीता सांख्यशास्त्र के प्रकृति-विश्लेषण के ही अंतर्गत बने रहने से संतुष्ट नहीं होती; क्योंकि यह विश्लेषण तो प्रकृति में केवल अहंभाव को ही स्थान देता है, बहु-पुरुष को नहीं - वहाँ वह प्रकृति का कोई अंग नहीं, अपितु प्रकृति से पृथक् है। इसके विपरीत गीता दृढ़तापूर्वक ऐसा स्थापित करती है कि परमेश्वर ही अपनी प्रकृति से जीव बनते हैं। यह कैसे संभव है जब विश्व-प्रकृति के केवल चौबीस तत्त्व हैं, अन्य और नहीं? दिव्य गुरु कहते हैं कि हाँ, वैश्व त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बाह्य कर्म का यही सही विवरण है और इस विवरण में पुरुष और प्रकृति का जैसा संबंध बताया गया है, वह भी बिल्कुल प्रामाणिक है और प्रवृत्ति या निवृत्ति के व्यावहारिक प्रयोगों में भारी उपयोग का भी है। परन्तु यह केवल त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति है जो अवचेतन और बाह्य है; इसके परे एक उच्चतर, परम, चैतन्य तथा दिव्य परा प्रकृति है, यही परा प्रकृति व्यष्टिगत आत्मा, जीव, बनी है। अपरा प्रकृति में प्रत्येक जीव अहंभावापन्न प्रतीत होता है, परा प्रकृति में प्रत्येक जीव व्यष्टिरूप पुरुष है। दूसरे शब्दों में बहुत्व उस 'एक' के ही आध्यात्मिक स्वभाव का एक अंग है। यह व्यष्टि-पुरुष, भगवान् कहते हैं कि, स्वयं मैं हूँ, इस सृष्टि में मेरी ही आंशिक अभिव्यक्ति है, 'ममैवांशः', और इसमें मेरी सब शक्तियाँ निहित हैं; यह साक्षी है, अनुमंता है, भर्ता है, ज्ञाता है, ईश्वर है। यह अपरा प्रकृति में उतर आता है और स्वयं को कर्म से बँधा मान लेता है, जिससे कि निम्न सत्ता को भोग सके : यह इससे निवृत्त होकर अपने को सभी कर्म-बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त अकर्ता पुरुष जान सकता है। यह तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है और, कर्म-बंधन से मुक्त हुआ भी कर्म कर सकता है, जैसे भगवान् कहते हैं कि मैं स्वयं करता हूँ, और पुरुषोत्तम की भक्ति के द्वारा और उनसे युक्त होकर पूर्ण रूप से उनकी दिव्य प्रकृति का आनन्द ले सकता है।
xv.7 , xiii 23
ऐसा है गीता का विश्लेषण जो अपने-आप को बाह्य (दृश्यमान) सृष्टि-क्रम या वैश्व-प्रणाली से ही बद्ध न कर के परा प्रकृति के 'उत्तमं रहस्यं' तक में भीतर प्रविष्ट हो जाता है। उसी उत्तम रहस्य के आधार पर गीता अपने वेदांत, सांख्य और योग के समन्वय को, ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय को स्थापित करती है। एकमात्र शुद्ध सांख्य के द्वारा ही कर्म और मुक्ति का संयोजन परस्पर-विरोधात्मक है और असंभव है। एकमात्र शुद्ध अद्वैत के आधार पर योग के एक अंग के रूप से कर्मों की स्थायी निरंतरता तथा पूर्ण ज्ञान, मुक्ति और सायुज्य प्राप्त होने के बाद भी भक्ति में अनुरक्ति असंभव हो जाती है या कम-से-कम युक्ति-विरुद्ध और निष्प्रयोजन हो जाती है। गीता का सांख्य-ज्ञान इन सब बाधाओं को दूर करता है और गीता की योग-प्रणाली इन सब पर विजय लाभ करती है।
[उपर्युक्त चर्चा के प्रकाश में] हम इस बात को समझ सकते हैं कि गीता क्यों उस विशिष्ट प्रतिपादन-शैली का अनुसरण करती है जो उसने अपनायी है। (वह शैली यह है कि) पहले किसी आंशिक सत्य का, उसके गंभीर अर्थ के कुछ मृदु-मंद संकेतों के साथ, निरूपण कर देना, और फिर आगे चलकर अपने इन संकेतों की ओर लौटना और उनके मर्म को अथवा गुढ़ार्थ को प्रकट करना, और ऐसा करते रहना जब तक कि वह इन सबके ऊपर उठकर अपने उस अंतिम महान् संकेत में, अपने उस परम रहस्य में नहीं पहुँच जाती जिसका वह स्वयं बिल्कुल भी निरूपण नहीं करती, अपितु उसको मनुष्य जीवन में अनुभूत होने के लिये छोड़ देती है, जैसे कि भारतीय आध्यात्मिकता के उत्तर युगों में प्रेम की, आत्मसमर्पण की और आनन्द की महान् लहरों में इसे अनुभूत करने का प्रयास किया गया। गीता की दृष्टि सदा अपने समन्वय पर है और उसमें जो विभिन्न विचारधाराओं का वर्णन है वह मानव-मन की उस अन्तिम परम वचन के लिये क्रमिक या उत्तरोत्तर तैयारी है।
यहाँ जो मुख्य बात है वह यह है कि जो पच्चीसवाँ तत्त्व है वह गीता में प्रकृति के अंदर ही आ जाता है। 'पराप्रकृतिर्जीवभूता' – एक है निम्न प्रकृति जो अपरा प्रकृति है, और दूसरी है परा प्रकृति। यह परा प्रकृति ही जीव बनती है। परंतु परा प्रकृति केवल जीव ही नहीं है, वह उससे भी अधिक बहुत कुछ है, वही पुरुष का रूप भी धारण करती है। ईश्वर की सारी अभिव्यक्ति उनकी परा प्रकृति में ही है। जबकि सांख्य में तो 'अहंकार' को ही पुरुष का रूप दे देते हैं। 'पराप्रकृतिर्जीवभूता' के अंदर अहंभाव तो प्रकृति का ही खेल है, वह पुरुष का रूप नहीं है। सच्चा पुरुष तो केवल एक ही है और वह कोई भी भाव ग्रहण कर सकता है – क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। इसलिए पारंपरिक सांख्य से अलग गीता ने एक के अंदर ही सारे को एकीभूत कर दिया है। हमें मूलतः जो बात समझने की है वह यह है कि गीता का योग न तो पतंजलि के समान ही कोई पारंपरिक योग है और न ही उसका सांख्य आम तौर पर समझे जाने वाला सांख्य ही है। गीता की अपनी ही एक अनूठी पद्धति है जो कि आगे चलकर तो बिल्कुल स्पष्ट ही हो जाएगी। क्योंकि पारंपरिक सांख्य और योग के आधार पर तो ऐसे भक्ति, कर्म तथा ज्ञानयोग संभव हो ही नहीं सकते जिनका प्रतिपादन गीता कर रही है। सांख्य-योग के अनुसार तो कर्मयोग संभव नहीं है और भक्तियोग भी संभव नहीं है। अतः ज्ञान और भक्तियोग का समन्वय भी नहीं हो सकता। परन्तु गीता का जो सांख्य और योग है वह इन सबका अतिक्रमण कर जाता है। उस सब को पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण में केंद्रीभूत कर दिया जाता है। ये सभी एकीभूत होकर उन्हीं में जा मिलते हैं।
III. बुद्धि योग
दिव्य गुरु अर्जुन से कहते हैं कि सांख्यों में आत्म-मुक्तिदायी बुद्धि की जो संतुलित अवस्था है वह, मैंने तुझे बता दी है। अब मैं योग में जो दूसरी संतुलित अवस्था या स्थिति है उसका वर्णन करूँगा। तू अपने कर्मों के फलों से भयवश सकुचा रहा है, तू कोई दूसरे ही फल चाहता है और अपने जीवन के सच्चे कर्म-पथ से हट रहा है क्योंकि यह पथ तुझे तेरे वांछित फलों की ओर नहीं ले जाता। परन्तु कर्मों और उनके फल का विचार, फल की कामना ही कर्म का हेतु होना, कामना की पूर्ति के साधन के रूप में कर्म करना उन अज्ञानियों का बंधन है जो यह नहीं जानते कि कर्म क्या हैं, न उनके सच्चे स्रोत को जानते हैं, न उनकी वास्तविक कार्यविधि, और न उनकी श्रेष्ठ उपयोगिता को ही जानते हैं। मेरा योग तुझे आत्मा के अपने कर्मों के समस्त बंधनों से मुक्त कर देगा.....
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।४०॥
४०. इस मार्ग पर कोई भी प्रयास नष्ट नहीं होता, न ही कोई प्रत्यागमन ही होता है, इस धर्म का थोड़ा-सा अनुष्ठान भी महान् भय से मुक्त कर देता है।
तू बहुत-सी चीजों से भयभीत है, पाप से भयभीत है, दुःख से भयभीत है, नर्क और दंड से भयभीत है, ईश्वर से भयभीत है और इस लोक से और परलोक से भयभीत है तथा अपने-आप से भयभीत है। ऐसी कौन-सी चीज है जिससे, हे आर्य योद्धा, जगत् के वीरशिरोमणि, तू भयभीत नहीं है? परन्तु यह महाभय ही तो मानव जाति को घेरे रहता है- लोक और परलोक में पाप और दुःख का भय, जिस संसार के सत्य स्वभाव को वह नहीं जानती उस संसार में भय, उस ईश्वर का भय जिसकी सत्य सत्ता को भी उसने नहीं देखा है और न जिसकी विश्वलीला के अभिप्राय को ही समझती है। मेरा योग तुझे इस महाभय से तार देगा और इस योग का स्वल्प-सा साधन भी तुझे मुक्ति दिला देगा। जब एक बार तूने इस मार्ग पर यात्रा शुरू कर दी तो तू देखेगा कि कोई कदम व्यर्थ नहीं रखा गया; प्रत्येक छोटी-से-छोटी गति भी एक वृद्धि अथवा प्राप्ति होगी; तुझे ऐसी कोई बाधा नहीं मिलेगी जो तेरी प्रगति में रुकावट पैदा कर सके। कितना निर्भीक और निरपेक्ष आश्वासन है। परन्तु एक ऐसा वचन जिस पर आक्रांत और सभी मार्गों में लड़खड़ाता भयभीत और शंकित मन सहसा ही अपना पूर्ण भरोसा नहीं रख सकता; और न ही इस प्रतिज्ञा का व्यापक और पूर्ण सत्य तब तक प्रत्यक्ष ही होता है जब तक गीता के प्रारंभिक वचनों के साथ उसका यह अंतिम वचन मिलाकर न पढ़ा जाएः
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। xviii.66
'सभी धर्मों का परित्याग कर के केवल एक मेरी ही शरण ग्रहण कर; मैं तुझे सब पापों और अशुभों से मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर।'
परन्तु भगवान् द्वारा मनुष्य को कहे इस गंभीर और हृदयस्पर्शी शब्द के साथ गीता का प्रतिपादन आरम्भ नहीं होता, अपितु आरंभ तो मार्ग पर चलने के लिये प्राथमिक रूप से आवश्यक कुछ प्रकाश की किरणों से होता है और वे भी आत्मा को लक्ष्य कर के निर्देशित नहीं की गई हैं अपितु बुद्धि को लक्ष्य कर के निर्देशित की गई हैं। शुरू में मनुष्य के सुहृद् और प्रेमी भगवान् नहीं बोलते हैं, अपितु वे भगवान् बोलते हैं जो उसके पथ-प्रदर्शक और गुरु हैं, जिन्हें शिष्य से उसकी सच्ची आत्मा, जगत् के स्वभाव अथवा स्वरूप तथा उसके अपने कर्म के उद्गमों के विषय में अज्ञान को दूर करना है। चूंकि मनुष्य अज्ञानपूर्वक और अशुद्ध बुद्धि के साथ और इस (अशुद्ध बुद्धि) के कारण से इन विषयों में अशुद्ध संकल्प के साथ कर्म करता है इसलिए वह अपने कर्मों से बंध जाता है या बद्ध प्रतीत होता है; अन्यथा मुक्त आत्मा के लिए कर्म कोई बंधन नहीं होते। इस अशुद्ध बुद्धि के कारण ही मनुष्य को आशा, भय, क्रोध और शोक तथा क्षणिक सुख होता है; अन्यथा पूर्ण शांति और स्वतंत्रता के साथ भी कर्म किये जा सकते हैं। इसलिए बुद्धि का योग ही है जो अर्जुन को बताया गया है। शुद्ध बुद्धि और फलतः शुद्ध संकल्प के साथ उस एक परमात्मा में स्थित होकर, सब में उस एक आत्मा को जानते हुए तथा उसको सम शांति से कार्य करते हुए और सतही मनोमय पुरुष की हजारों उमंगों के वश इधर-उधर भटके बिना कर्म करना ही बुद्धियोग है।
गीता ने एक ऐसी चीज का प्रतिपादन किया है जो सहज ही सामान्य बुद्धि की समझ में नहीं आ सकती। हमारी बुद्धि जिस तरह का संसार देखती है, जिस तरह के क्रिया-कलाप देखती है, उसमें सारे दिन अच्छी चीजों के बाद बुरे परिणाम आते दिखाई देते हैं, ऐसे में व्यक्ति इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता है कि वह हमेशा आगे ही बढ़ता जाएगा और कभी प्रत्यावर्तन नहीं होगा क्योंकि जिन्हें शुभ या धार्मिक कार्य कहा जाता है उनमें भी बाधा आ जाती है, विनाश हो जाता है, और तब उसके लिए इस कथन पर विश्वास करना आसान नहीं है। हालाँकि इस पर विश्वास किए बिना आगे चलने का अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। परंतु विश्वास करने में समस्या यह है कि भले ही हमारी आत्मा तो इस बात को जानती है, विश्वास कर सकती है, पर अभी वह ऐसी बुद्धि द्वारा आच्छादित होती है जो अशुद्ध है और अशुद्ध बुद्धि के कारण आत्मा की क्रिया भी दूषित हो जाती है। इसलिए गीता उस बुद्धि के भ्रम को दूर करने के प्रयास से आरंभ करती है जो बाह्य प्रतीतियों से भ्रमित हो जाती है और उस कारण विश्वास नहीं कर पाती। बुद्धि के लिए कैसे संभव है कि वह इस वाक्य पर विश्वास कर पाए कि 'इस मार्ग पर रखे कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाते और सदा उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है।' इसलिए गीता सर्वप्रथम बुद्धि की गाँठों को खोलना आरंभ करती है, जो कि सहज नहीं है। दूसरे अध्याय से ये गाँठें खुलनी आरम्भ हो जाती है। उसके बाद आगे से आगे प्रश्नों और शंकाओं का समाधान होता जाएगा। एक पड़ाव पर आकर अर्जुन बुद्धि से तो समझ जाता है परंतु जब तक उस ज्ञान का उसे सजीव अनुभव न हो तब तक उसमें वह शक्ति नहीं आ पाती। तब फिर वह उसके अनुभव प्राप्त करने की चाह करता है। अब गीता बुद्धियोग का निरूपण करेगी क्योंकि ये संदेश केवल आत्मा ही समझ सकती है। वास्तव में तो सारी गीता का चलन केवल इसी तरह है कि एक गुरु के रूप में शिष्य को दिये जा रहे संदेश की अपेक्षा एक प्रेमी के रूप में दिये जाने वाले संदेश 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' को सुनने के लिए और उसे आत्मसात् करने के लिए अर्जुन को तैयार किया जा सके। सारी गीता की तैयारी ही इस बात की है कि अर्जुन की बुद्धि को तथा अन्य अंगों को इतना तैयार कर दिया जाए कि और कोई आवरण न रह जाए और यह संदेश उसे दिया जा सके। अपने जीवन में भी हम यही चीज देख सकते हैं। प्रभु की लीला को हम समझ नहीं सकते। हम कल्पना करते हैं कि हमें भली-भाँति समझ में आ गया है कि हमारे इष्ट के अतिरिक्त, श्रीमाँ-श्रीअरविन्द के अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है और उनका अनुकरण करना ही एकमात्र करने योग्य कार्य है। हमारा नैतिकता का बोध भी इसे ही सही ठहराता है। परन्तु समस्या यह है कि ये सभी भाव अधिकांशतः हमारे मानसिक रूपण मात्र होते हैं। हालाँकि आत्मा इन सबके द्वारा कार्य कर रही होती है, परंतु हमारे विकास को तब तक गति नहीं मिलती जब तक कि हमें इसका जीवंत अनुभव नहीं आ जाता कि इसमें किस प्रकार का आकर्षण है। जैसे पतंगा स्वयं जल भले ही जाए, फिर भी रुक नहीं सकता और आग की ओर अनायास ही चला जाता है, वैसे ही हमारे अंदर इस प्रकार का प्रवाह आता है कि हम उसे रोक ही नहीं सकते। परंतु परमात्मा का प्रेम तो इससे भी सर्वथा भिन्न प्रकार का होता है। वह तो नित्य-निरंतर है, अहैतुक है, जिसका कोई कारण नहीं है। वहीं, यदि व्यक्ति अपने किन्हीं भागों में तो कुछ-कुछ समझा है कि उसे अपने इष्ट का अनुकरण करना है, या फिर उसे किसी उद्देश्य के प्रति कोई आकर्षण प्राप्त हुआ है - हो सकता है कि प्राण ज्वलंत रूप से किसी उद्देश्य के लिए अभिप्रेरित हो जाए, मन किसी आदर्श के प्रति आकृष्ट हो जाए - तो भी इन सब में उस दिव्य प्रेम के सहज आकर्षण का गुण नहीं होता। और जब तक वह जागृत नहीं होता तब तक हमारे अहम् आदि सभी स्थूल या सूक्ष्म रूप से हावी रहते हैं, और परमात्मा से सच्चा एकत्व स्थापित नहीं हो सकता और न ही व्यक्ति को अपनी सच्ची आंतरिक शक्ति का भान हो सकता है। जब वह स्थापित हो जाता है तब फिर विशेष कुछ व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता नहीं रह जाती, वह तो स्वयं ही सभी प्रतिकूल चीजों को जला कर भस्म कर देता है। गीता उसी की ओर ले जाती है और वहाँ तक ले जाकर छोड़ देती है। जब आत्मा की वह प्रवृत्ति अन्दर जागृत हो गई तब कोई चीज हमें विचलित कर सके यह तो संभव ही नहीं है। हमारे ऋषि भी, जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन का अनुभव किया, यही बात कहते हैं कि साधना आदि तो सब तैयारी मात्र हैं। एक बार जब वह गति आरंभ हो जाए तब फिर अन्य कोई पद्धति या प्रणाली उसमें कुछ नहीं कर सकती और उनकी उपयोगिता भी नहीं रह जाती। जिस प्रकार चुंबक की प्रकृति मात्र ही है लोहे को अपनी ओर आकृष्ट करना और लोहे की प्रकृति है अनायास ही उसकी ओर खिंचे चले जाना, इसमें किसी पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा की वह गति चालू होने के बाद तो अन्य किन्हीं भी पद्धतियों की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिए वास्तव में तो गीता की सारी व्यवस्था ही पहले वचन से लेकर अन्ततः 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' तक ले जाने का आरोहण-क्रम मात्र है। और वास्तविक कार्य तो उसके बाद शुरू होता है। श्रीअरविन्द कहते हैं कि सारी गीता मनुष्य की आत्मा को उसी के लिए तैयार करने के लिए है ताकि उस पर पड़े बुद्धि के, भ्रम के, अनुभवों के आवरणों को हटाकर उसे उस स्तर तक ले जाया जा सके। इस प्रकार गीता के पूरे क्रम को देखने का यह एक दृष्टिकोण है।
अब, बुद्धि के अंदर, इच्छा-शक्ति के अंदर कुछ प्रवृत्तियाँ रहती हैं कि यह प्राप्त कर लिया जाए, वह प्राप्त कर लिया जाए। इन सबके विषय में भगवान् अर्जुन को समझाने वाले हैं, परंतु ये बातें सहज ही उसे समझ में नहीं आएँगी जिस कारण प्रश्न भी उठेंगे, क्योंकि केवल बताने भर से ही ये बातें समझ में नहीं आ जातीं। आध्यात्मिक जीवन में केवल पुस्तक पढ़ने से और प्रवचन सुनने से बातें समझ में नहीं आ जातीं। हमारी बुद्धि में बहुत तरह की मानसिक संरचनाएँ तथा वृत्तियाँ जमी बैठी होती हैं। इन सबको नष्ट करना होगा। तब धीरे-धीरे अनुभव आता है, और श्रद्धा ऊपर आती है। साधना में इसीलिए इतना समय लगता है। पर कुछ ऐसे परिपक्व लोग भी होते हैं जिनका वह भाव पहले से ही तैयार होता है और जब उसे उद्घाटित कर दिया जाता है तब फिर उनकी साधना त्वरित रूप से संपन्न हो जाती है। वास्तविक समझ भी तभी आती है।
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।
बहुशाखा ह्यनन्ताश्व बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ।।४१।।
४१. हे कुरुनन्दन (अर्जुन)! इस मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि एकनिष्ठ होती है; परंतु अनिश्चित चित्तवाले मनुष्यों की बुद्धि अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती है।
गीता कहती है कि मनुष्य में दो प्रकार की बुद्धि होती है। पहली होती है एकाग्र, संतुलित, एकनिष्ठ, समरस, केवल परम सत्य की ओर ही लक्षित; एकत्व उसकी विशिष्टता है और एकाग्र स्थिरता उसका स्वरूपमात्र। दूसरी में कोई एकनिष्ठ संकल्प नहीं होता, कोई एकीकृत बुद्धि नहीं, अपितु केवल अनेक शाखा-प्रशाखायुक्त असंख्य विचार हैं जो भाग-दौड़ कर रहे हैं, अर्थात् जीवन और परिवेशजन्य इच्छाओं की तुष्टि के पीछे इधर-उधर भटक रहे हैं। जिस बुद्धि शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, शुद्ध अर्थ में उसका आशय है समझने-बूझने की मानसिक शक्ति, किन्तु स्पष्ट रूप से गीता में बुद्धि शब्द का प्रयोग व्यापक दार्शनिक अर्थ में उस मन की समस्त विवेकात्मक और निर्णयकारी क्रिया हेतु हुआ है जो (मन) हमारे विचारों की दिशा और उनके प्रयोग तथा हमारे कर्मों की दिशा और उनके प्रयोग, इन दोनों बातों का निर्धारण करता है; विचार, समझ-बूझ, निर्णय, बोधयुक्त चयन और लक्ष्य-साधन ये सब बुद्धि की क्रिया में सम्मिलित हैं : क्योंकि एकीकृत बुद्धि का लक्षण केवल बोधयुक्त मन का केंद्रीकरण ही नहीं है, अपितु उस मन का भी केंद्रीकरण है जो निर्णय करने वाला और उस निर्णय अर्थात् व्यवसाय पर अटल रहने वाला है, दूसरी ओर अव्यवसायात्मिका बुद्धि का लक्षण उसके विचारों और बोधों की असंबद्धता या भटकाव उतना नहीं है जितना उसके लक्ष्यों और उसकी इच्छाओं का और फलतः उसके संकल्प की असंबद्धता या इधर-उधर भटकाव है। अतः संकल्प और ज्ञान, बुद्धि की ये दो क्रियाएँ हैं।
गीता यहाँ दो भेदों का निरूपण करती है। बुद्धि सही तभी है जब उसने सोच-विचार कर अपने विवेक से एक निर्णय कर लिया और उस पर चलती है अन्यथा तो बुद्धि है ही नहीं, वह तो केवल एक भटकाव है क्योंकि किसी भी समय भिन्न-भिन्न इच्छाएँ और विचार आकर उस पर अधिकार कर लेते हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति को यह बोध हो भी कि केवल श्रीमाताजी की सेवा ही करनी है तो भी जो कोई भी अन्य भाव या प्रवृत्ति उठती है वही उस पर अधिकार जमा लेती है। इसलिए बोध तो सही होता है परंतु इच्छा-शक्ति में भटकाव रहता है। यह है अव्यवसायात्मिका बुद्धि। उससे मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। क्योंकि उसका संकल्प विचलित होता रहता है, और ऐसे में जितना वह आगे जाता है उतना ही लौट कर पुनः पीछे आ जाता है। बीच में ही संदेह घुस आता है, क्योंकि मार्ग कोई भौतिक चीज तो है नहीं, यह तो श्रद्धा का विषय है। व्यक्ति की श्रद्धा जितनी ही अक्षुण्ण बने रहेगी उतना ही मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। जब उसमें भटकाव आता है तब फिर वह पथभ्रष्ट करके किसी अन्य दिशा में ले जाता है और ऐसे में व्यक्ति कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए अव्यवसायात्मिका बुद्धि वह है जो हमारी संकल्प-शक्ति को एक स्थान पर नियत नहीं रख सकती। उचित क्या है केवल इसका बोध होना ही पर्याप्त नहीं है - हालाँकि बोध भी नहीं हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति मार्ग पर है ही नहीं - परन्तु बोध होने पर भी यदि संकल्प-शक्ति में भटकाव हो तो कुछ भी संसिद्ध नहीं किया जा सकता।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।॥४२॥
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।।४३।।
४२-४३. हे पार्थ! अविवेकी, वेद के मतवाद में रत, ऐसा मानने वाले कि इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कामनायुक्त चित्तवाले, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिये परिश्रम करने वाले मनुष्य कर्मों के जन्मरूप फल को देनेवाली, भोग और ऐश्वर्य को लक्ष्य में रखनेवाली, विशिष्ट प्रकार की बहुत-सी क्रियाओं वाली इस प्रकार की सुनने में रोचक वाणी को कहते हैं।
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।।४४।॥
४४. इस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हरा गया (भ्रांत कर दिया गया) है और जो भोग एवं ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उनकी बुद्धि एकाग्रचित्तता के साथ (समाधिस्थ हो) आत्मा में प्रतिष्ठत नहीं होती।
त्रैगुण्यविषया वेदा निखैगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ।।४५।।
४५. हे अर्जुन! समस्त वेदों का विषय तीन गुणों का कार्य-व्यवहार है; परंतु तू तीन गुणों से मुक्त (त्रिगुणातीत), द्वन्द्वों से रहित (निर्द्वन्द्व), सदा अपने सच्चे आत्मा में स्थित, पदार्थों की प्राप्ति और उन्हें अधिकार में सुरक्षित रखने की चिंता से रहित हो, आत्मा को प्राप्त कर।
---------------------
* सांख्य प्रणाली में ये तीन स्थितियाँ अथवा गुण दिये गये हैं... ये तीन नाम हैं, सत्त्व, रजस्, और तमस्। तमस् जड़त्व अथवा निष्क्रियता का तत्त्व एवं उसकी शक्ति है, रजस् गति अथवा क्रिया, आवेश, प्रयत्न, संघर्ष और आरम्भ का तत्त्व है; सत्त्व समावेशीकरण, सन्तुलन और सामंजस्य का तत्त्व है। हमारे अन्दर होनेवाले कर्म और अनुभव का समस्त स्वरूप प्रकृति के इन तीन गुर्गों या स्थिति में से किसी एक को प्रधानता एवं इनको आनुपातिक परस्पर प्रतिक्रिया के द्वारा निर्धारित होता है। व्यष्टिभावापन्न आत्मा इनके साँचे में ढलने के लिये मानो बाध्य होती है; साथ ही इन पर किसी प्रकार का स्वतन्त्र नियन्त्रण रखने की अपेक्षा अधिकांशतः वह इनके नियन्त्रण में ही रहती है। वह मुक्त तभी हो सकती है जब वह इनकी विषम क्रिया तथा इनके अपर्याप्त मेल-मिलापों एवं अनिश्चित सामंजस्यों के कष्टप्रद कलह की स्थिति से ऊपर उठकर उसका परित्याग कर दे...
* निम्न प्रकृति में द्वंद्व सात्त्विक, राजसिक और तामसिक अहं की रचनाओं से अभिभूत आत्मा पर गुणों की क्रीड़ा का अनिवार्य प्रभाव हैं। इस द्वंद्व को ग्रन्थि है अज्ञान जो पदार्थों के आध्यात्मिक सत्य को पकड़ पाने में असमर्थ है और अपूर्ण बाह्य रूपों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, पर उनके आन्तरिक सत्य पर प्रभुत्व रखते हुए उनका सामना या उनसे व्यवहार नहीं करता अपितु आकर्षण और विकर्षण, सामर्थ्य और असामर्थ्य, राग और द्वेष, सुख और दुःख, हर्ष और शोक, स्वीकृति और घृणा के बीच संघर्ष और एक-दूसरे में बदलते हुए सन्तुलन के साथ उनके सम्पर्क में आता है: समस्त जीवन हमारे सामने इन वस्तुओं अर्थात् प्रिय और अप्रिय, सुन्दर और असुन्दर, सत्य और असत्य, सौभाग्य और दुर्भाग्य, सफलता और विफलता, शुभ और अशुभ की विषम ग्रन्थि या प्रकृति के दुहरे जटिल जाल के रूप में उपस्थित होता है। अपनी रुचियों और अरुचियों के प्रति आसक्ति अन्तरात्मा को शुभ और अशुभ तथा हर्षों और शोकों के इस जाल में बाँधे रखती है। मुक्ति का अन्वेषक अपने-आपको आसक्ति से मुक्त कर लेता है, द्वंद्वों को अपनी अन्तःसत्ता से दूर फेंक देता है..
* क्योंकि मुक्त पुरुष के लिए (योगक्षेम) प्राप्ति और अधिकारोक्ति क्या हैं? जहाँ एकबार हम आत्मवान् हुए वहीं सब कुछ तो प्राप्त हो जाता है।
कर्म और ज्ञान के समन्वय का लगभग पहला ही कथन, वेदवाद की एक कठोर, और प्रायः एक प्रचंड निन्दा और खण्डन है।.. यहाँ तक कि गीता स्वयं वेद पर आक्रमण करती प्रतीत होती है, जिसका यद्यपि भारतीय समाज के व्यवहार में इस समय लोप ही हो गया है, तो भी भारतीय समाज की भावना में वेद अब भी समस्त भारतीय दर्शन-शास्त्रों और धर्मों के अप्रत्यक्ष, अनुल्लंघनीय, अत्यंत पवित्र और स्वतःसिद्ध प्रमाण और मूल हैं।... सब वेद उस मनुष्य के लिये निष्प्रयोजन बताये गये हैं जो ज्ञानी है। यहाँ वेदों, 'सर्वेषु वेदेषु', में उपनिषदों का भी समावेश माना जा सकता है और कदाचित् है भी, क्योंकि आगे चलकर वेद और उपनिषद्, दोनों के सामान्य वाचक श्रुति शब्द का ही प्रयोग हुआ है।
यहाँ प्रश्न यह है कि सत्त्व, रजस् और तमस् किस तरीके से आत्मा को बाँधते हैं, और अपने-आप में इनका स्वरूप क्या है? इसे देखने का एक दृष्टिकोण तो यह है कि बद्ध जीव को, जो सारे दिन यंत्रवत् चालित है, तो यह अंदेशा तक भी नहीं होता कि आत्मा जैसी किसी चीज का अस्तित्व भी है, तो बँधे होने के बोध की बात तो उठती ही नहीं। पहले ऐसी किसी ऐसी चीज का भान होना आवश्यक है जिसे कि सत्त्व, रजस् और तमस् तीनों ने बाँध रखा हो। एक विशालतर परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम किस हद तक बँधे हुए हैं इस बात का पता तो इसी से लग जाता है कि आत्मा के होने के बावजूद भी हम वस्तुओं को उनके आत्म-स्वरूप में न देखकर कितने भिन्न या फिर उनके विपरीत रूप में देख रहे हैं। यदि गुरु की कृपा हो या जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जो हमें इसका भान करा दे कि आत्मा जैसी किसी चीज की सत्ता है, और हम उसके संपर्क में आ जाएँ तब यदि हम ध्यान से देखें तो पता चल सकता है कि किस प्रकार सारे क्रिया-कलाप में तमस् अपना प्रभाव डालता है, रजस् अपना रंग चढ़ा देता है और सत्त्व अपना प्रभाव डाल देता है। तमस् अपनी निष्क्रियता, भारीपन, किसी कार्य में उत्साह के अभाव का रंग डाल देता है। रजस् अपनी क्रियाशील प्रकृति को, अपनी इच्छाओं, वासनाओं, अधिकार जमाने के रंगों को उसके अन्दर डाल देता है। सत्त्व अपने विचारों को और जैसा भी उसका अपना स्वरूप है उस अनुसार सभी कुछ को रंग देता है। ऐसे में हम वैसा आचरण करने लगते हैं जो हमारे निजस्वरूप से भिन्न या विपरीत होता है। सारे समय हम अपने शारीरिक सुख-भोगों को भोगने का प्रयत्न करते हैं, अपनी इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं या फिर अपने विचारों आदि को थोपने की तथा पोषित करने की कोशिश करते हैं। तो यदि यह विचार लें कि जीव इस अभिव्यक्ति में शरीर धारण कर के आया है, भले उसका जो भी गहरा कारण रहा हो, परंतु फिर भी वर्तमान में जो प्रतीति है उसमें तो हम अपने सच्चे स्वरूप से बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। और इसी को कहा जा सकता है कि सत्त्व, रजस् और तमस् ने हमें इससे बाँध दिया है।
यह सब वर्णन तो इस संबंध में हुआ कि किस प्रकार ये हमारी आत्मा को बाँधते हैं। अब जो दार्शनिक प्रश्न रह जाता है वह यह है कि ये तीन गुण वास्तव में क्या हैं? और अभिव्यक्ति में ये आए कैसे? श्रीअरविन्द ने लिखा है कि बहुत अधिक सूक्ष्म निरीक्षण करने पर इनका बोध होता है, अन्यथा तो इनका बोध ही नहीं होता। तब फिर सत्त्व, रजस् और तमस् की परिकल्पना या यह विचार आया कहाँ से? इसके बारे में श्रीअरविन्द परोक्ष रूप से या कहीं-कहीं प्रसंगवश थोड़ा-सा संकेत करते हैं। परन्तु अपने अनुभव से हम इनके स्वरूप को अधिक जान सकते हैं। समझने के इस प्रयत्न का लाभ इतना ही है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम इनके विषय में कुछ अधिक सचेतन होंगे और अधिक बेहतर तरीके से इनके ऊपर नियंत्रण और क्रिया कर सकेंगे।
भगवान् के अनन्त गुण हैं, एक अतिमानसिक सत्य है जो इस क्रमविकासमय अभिव्यक्ति के अंदर अपने को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। हालाँकि हम तो भगवान् के केवल कुछ ही गुणों के विषय में सचेतन हैं, परंतु प्रकृति में तो अन्य सभी गुणों को भी अभिव्यक्त करने का प्रयास चल रहा है। अंततः तो ये सारे ही गुण, जो कि इस जगत् के मूल में निहित हैं, एक निश्चित संतुलन में इस जगत् में अभिव्यक्त होने ही चाहिये। दूसरे जगतों की या ब्रह्माण्डों की क्या प्रणाली होगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस व्यवस्था में गुणों का हमें इस प्रकार बोध होता है, अन्य व्यवस्थाओं में यह कैसा होता होगा यह हम नहीं जानते। यदि अनन्त गुणों को देखा जाए और यह देखा जाए कि कौन से मनुष्य में कौन से गुण प्रभावी हैं तो इतनी व्यापक दृष्टि से देख पाना तो असंभव-सा होगा। इसलिए इन गुणों के खेल को तीन श्रेणियों में बाँट दिया गया। अब ये श्रेणियाँ कहाँ से आईं? भगवान् की चेतना मनुष्य में उन गुणों को लाकर उन्हें आविर्भूत करने का प्रयास करती है। जब वह जड़-भौतिक तत्त्व में अपना प्रभाव डालती है तब उसके प्रति जड़-तत्त्व की प्रतिक्रिया अपने तरीके की होती है। उसे तमस् की संज्ञा दे दी जाती है। परंतु केवल जड़-तत्त्व में ही नहीं, उस चेतना को तो मन, प्राण और शरीर तीनों के ही द्वारा अभिव्यक्त होना होता है। अतः जब वह प्राण के द्वारा अभिव्यक्त होती है तो प्राण की प्रतिक्रिया से उसमें गतिशीलता या क्रियाशीलता का तत्त्व आ जाता है। इसमें जड़त्व की स्थिरता का गुण कम रहता है। जब वह चेतना मन में प्रभाव डालती है तो मन चीजों में संतुलन को देखता है। यह सत्त्व का तत्त्व होता है। पर ये सभी कोई नियत-निर्धारित चीजें नहीं हैं। किसी एक व्यक्ति का तमस् दूसरे व्यक्ति के तमस् से भिन्न होता है। हमारे कोष भिन्न-भिन्न हैं, क्षमताएँ भिन्न-भिन्न हैं। कुछ में गुण इतने सक्रिय होते हैं कि उनके भौतिक में भी वे अभिव्यक्ति पाते हैं जबकि दूसरों में वे अंधकार में सुषुप्त रहते हैं। इसी प्रकार की बात मन पर भी लागू होती है। जैसी संरचना होगी वैसा ही आधान या प्रतिबिंब उस चेतना का या उस प्रकाश का होगा। गुणों का परस्पर सम्मिश्रण भी उसी के अनुसार रहेगा। परंतु यह तो देखने और समझने का केवल एक तरीका मात्र है। तो इन तीनों का क्रियाकलाप इस प्रकार का है। इन सब गुणों का जिस प्रकार हमें बोध होता है, हमें ये जिस प्रकार या जिस रूप में दिखाई देते हैं वह केवल इसलिए है क्योंकि हमारी चेतना मानसिक चेतना है। वस्तुतः अपने-आप में तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। वास्तव में तो यह सारा परा-प्रकृति का, दिव्य जननी का ही खेल है, अपरा प्रकृति है ही नहीं, अपरा प्रकृति तो हमें हमारे वर्तमान गठन के कारण प्रतीत होती है, अन्यथा गुणों का अस्तित्व ही नहीं है। चूंकि परा-प्रकृति की क्रिया को हमारा मन और अधिक समझ नहीं सकता, वह उसे केवल अपरा प्रकृति की प्रत्यक्ष क्रीड़ा या कार्य-व्यवहार के रूप में ही देख सकता है और उसका बोध प्राप्त कर सकता है, वैसे ही जैसे कि किसी बच्चे को कही किसी बात का वास्तविक अर्थ बच्चा क्या समझता है उससे सर्वथा भिन्न हो सकता है। वैसे ही यह सारा खेल परा प्रकृति का ही है परन्तु हमारे मन के अन्दर इसका जिस प्रकार का बिंब बनता है वैसा ही हमें यह समझ में आता है। और चूंकि परा-प्रकृति के पीछे तो स्वयं भगवान् की जो समस्त क्षमताएँ हैं, उनका व्यक्तित्व है, अतः उनकी अभिव्यक्ति को मनुष्य का मन समझ ही क्या सकता है, इसी कारण वह इस प्रकार के बिंब, इस प्रकार के रूपण तैयार करता है। परन्तु अपरा प्रकृति के अन्दर हमारे शरीर, प्राण और मन के अपने-अपने जो गुण 3-79^ 4pi , क्रियाशीलता और समता या विवेक - वे भगवान् के सच्चिदानंद स्वरूप से ही आए हैं, सत् जड़-तत्त्व बन जाता है, चित् के अंदर चित् और तापस दो पहलू हैं जिनमें तपस् प्राण बन जाता है और चेतना या ज्ञान पक्ष मन बन जाता है, आनंद आत्मा का गुण बन जाता है। ये चारों ही अभिव्यक्त हुए हैं। सच्चिदानंद के ये तीनों गुण अतिमानस में भी प्रक्षिप्त होते हैं तो वहाँ ये अलग-अलग रूप ले लेते हैं। स्थिरता का जो तत्त्व है वह बन जाता है 'समता'। प्राण बन जाता है तपस् और तीसरा तत्त्व बन जाता है ज्योति। वे ही चीजें यहाँ मन, प्राण और शरीर में इस रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। परंतु इन सब के पीछे अनन्त क्षमताएँ हैं। और भगवान् के व्यक्तित्व की, उनके सत्य की अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न मनुष्यों में भिन्न-भिन्न तत्त्वों के अनुसार होती है। उसी के आधार पर उसकी क्रियाकलाप का आकलन किया जा सकता है।
परंतु अब प्रश्न यह है कि निसैगुण्य होने की क्या आवश्यकता है? शंकराचार्य आदि का यह तर्क है कि यद्यपि भगवान् निसैगुण्य होने के लिए उपदेश कर रहे हैं परंतु जब भगवान् स्वयं भी अवतरित होते हैं तब उनके कर्म भी गुणों के अंतर्गत ही होते हैं, इसलिए मायावाद का निष्कर्ष यही है कि कर्म तो तैयारी करने के साधन मात्र हैं। और जब वह तैयारी पूरी हो जाती है तब उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। परंतु जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक भगवान् को भी अवतार लेकर क्रिया करने के लिये गुणों का, अज्ञान का बाना पहनना ही पड़ेगा। परंतु इसमें श्रीअरविन्द का मत इससे भिन्न है। भले ही हमें अवतार की क्रियाएँ भी त्रिगुणों से बद्ध नजर आएँगी, श्रीमाताजी की क्रियाएँ भी त्रिगुणों से बद्ध प्रतीत होंगी परंतु ऐसा तो हमें हमारी इंद्रियों के कारण प्रतीत होता है। वास्तव में तो उनमें दिव्य पराप्रकृति ही क्रिया कर रही होती है। चूंकि हमारी आँखों पर अज्ञान का आवरण चढ़ा होता है इसलिए हमें उनकी क्रियाएँ गुणों से बंधी हुई दिखाई देती हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है ही नहीं। वैसे ही अवतारों का इन गुणों से कोई सरोकार नहीं, भले उनकी क्रियाएँ गुणों की क्रीड़ा के वशीभूत प्रतीत होती हों। गुणों से अतीत होने का अर्थ है कि हम अपनी चेतना को इतनी विकसित कर लें कि हम सत्य को देख सकें। हम यह देख सकेंगे कि ये अनंत गुण किस प्रकार अभिव्यक्त हो रहे हैं और इनकी क्या व्यवस्था है, तब हम इनमें लिप्त नहीं होंगे क्योंकि हम सर्वत्र ही दिव्य परा-प्रकृति की क्रिया को ही देखेंगे। तब इन तीन गुणों का भ्रम नहीं रहेगा, क्योंकि वास्तव में तो गुणों का अस्तित्व ही नहीं है। यह तो दिव्य ऊर्जा की क्रिया को बोध करने का हमारा एक तरीका मात्र ही तो है। अतः इस प्रकार के बोध को जाना चाहिये और इसके स्थान पर स्पष्ट रूप में हमें महाशक्ति की क्रिया दिखाई देनी चाहिये। तब सारा परिदृश्य ही पूर्णतः बदल जाता है और एक नवीन रूप धारण कर लेता है। तब फिर प्रकाश, तपस् और समता, ये तीनों ही हमारे अन्दर आ जाएँगी। भगवान् इनके द्वारा अपनी क्रिया करेंगे। पर आखिर यह भी देखने का एक तरीका मात्र ही है, क्योंकि वास्तव में तो वे इन सभी से सर्वथा परे हैं।
दूसरा, जब चेतना विकसित नहीं होती तब हम द्वन्द्वों के द्वारा क्रिया करते हैं। यदि पसंदीदा और नापसंदीदा, अच्छी-बुरी जैसी चीज न हो तो हमारे पास कर्म के चयन का आधार नहीं रहता। क्योंकि सामान्यतः इन्हीं के आधार पर तो हम चीजों का चयन करते हैं। जबकि चयन करने का आधार होना चाहिए करणीय और अकरणीय का बोध। वह विवेक तो हमारे अंदर प्रायः होता ही नहीं और हम पसंद-नापसंद आदि द्वंद्वों के द्वारा ही प्रतिक्रिया करते हैं। एक पशु को भी हम अपनी सहजवृत्ति के द्वारा अपने-आप को पोड़ा से बचाते हुए देखते हैं और उसी के अनुसार वह अपनी प्रतिक्रियाएँ करता है। परंतु इस प्रकार की प्रतिक्रिया ही अंतिम हो, या चरम हो ऐसा नहीं है। हमारी प्रतिक्रिया अज्ञानमय नहीं अपितु सज्ञान होनी चाहिये। उदाहरण के लिये, यदि किसी नाटक में हम अपना भाग निभा रहे हैं तो हमारी क्रियाएँ तथा प्रतिक्रियाएँ वैसी होनी चाहिये जैसी उस नाटक की कथावस्तु के अनुकूल हों। जब तक हम द्वंद्वों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं तब तक समुचित रूप से कर्म नहीं कर सकते। समुचित रूप से कर्म तभी हो सकता है जब हम इन द्वंद्वों के प्रति समान भाव रखें, और जिस समय जैसा आवश्यक हो वैसा कर पायें। मूलभूत रूप से तो यदि हम पसंद-नापसंद से ऊपर हों तभी सही क्रिया का चयन कर पाएँगे अन्यथा तो हम जो पसंदीदा होगा वह करेंगे और जो नापसंद होगा उसे नहीं कर पाएँगे, और जो पसंदीदा है उसे भी हम तटस्थ रूप से नहीं निभा पाएँगे। जगदम्बा या दिव्य पराप्रकृति की क्रिया के प्रति हमारी सच्ची प्रतिक्रिया तभी होगी जब हम इन द्वन्द्वों के बारे में उदासीन हों, द्वन्द्वातीत हों। यदि अवतार द्वन्द्वों से बँधकर कर्म करे तब तो उसे हम प्रकृति के अधीन की कहेंगे, जबकि वास्तव में वह उससे ऊपर होता है।
यदि हमें भगवान् की ओर जाना है तो वे कहते हैं कि मैं इसलिए अवतार लेता हूँ ताकि मनुष्य मेरे उदाहरण को देखें। और उदाहरण यह है कि वे द्वन्द्वातीत हैं और गुणातीत हैं। अतः हमें भी अपरा को छोड़ कर दिव्य परा प्रकृति में क्रिया करने के लिए इनसे परे उठना पड़ेगा। अन्यथा कार्य का चयन सुख-दुःख, अच्छा-बुरा, श्रेष्ठ-निम्न आदि द्वन्द्वों के अनुसार होगा और ये सब मानदंड सीमित हैं। यदि परम मानदंड से कार्य करना हो तो इन सब से ऊपर उठना आवश्यक है। यह देखने का एक तरीका है। और यह सारी गुण आदि की शब्दावली भारत ने ही उत्पन्न की है, अन्यत्र कहीं तो यह है ही नहीं। हमारे ऋषियों ने भगवान् के अनन्त गुणों का बोध किया और देखा कि उसका वर्गीकरण, उसका प्रणालीकरण या उसका व्यवस्थापन किस प्रकार किया जाए। इसलिए सत्त्व, रजस् और तमस्, ये तीन मोटे विभाग बाँट दिये गये। उस चेतना के प्रति भौतिक जिस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है उसे तमस् की, प्राण-शक्ति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया करती है उसे रजस् की, और मन जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है उसे सत्त्व की संज्ञा दे दी गई। तीनों के अलग-अलग स्वरूप हैं। एक में स्थिरता या निष्क्रियता है, दूसरे में गतिशीलता या सक्रियता है और तीसरे में सामंजस्य का तत्त्व है। सत्त्व के आविर्भाव से हम क्रिया को व्यापक रूप से देख सकते हैं। इसी के अंदर तर्कशक्ति, बुद्धि आदि निहित हैं। इसलिए यह एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से क्रियाओं से दूर हटकर उन पर नजर डाली जा सकती है और फिर उन पर क्रिया की जा सकती है।
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके ।
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ।।४६।।
४६. सब ओर से पानी की बाढ़ आ जाने पर कुएँ में जितना प्रयोजन रह जाता है, उतना ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त किये हुए मनुष्य का समस्त वेदों में रह जाता है।
यही नहीं, अपितु शास्त्र-वचन तो बाधक भी होते हैं; क्योंकि शास्त्र के शब्द - कदाचित् इसके मूलपाठों के बीच भिन्नता और उनकी विविध और परस्पर विसम्मत व्याख्याओं के कारण बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, जो केवल अंदर की ज्योति से ही निश्चित मति और एकाग्र चित्तता प्राप्त कर सकती है।... यह सब परम्परागत धार्मिक भावना के लिये इतना अप्रिय या आपत्तिजनक होता है कि अपनी सुविधा देखनेवाली और अवसर से लाभ उठानेवाली मानव-प्रवृत्ति का गीता के कुछ श्लोकों के अर्थ को तोड़-मरोड़ कर उनका कुछ और अर्थ करने का प्रयास करना स्वाभाविक ही था, किन्तु इन श्लोकों का अर्थ अपने-आप में सुस्पष्ट है और आद्योपांत सुसंबद्ध है। शास्त्र-वचन-संबंधी यह भाव आगे चलकर एक और श्लोक में मंडित और सुनिर्दिष्ट हुआ है जहाँ यह कहा गया है कि ज्ञानी का ज्ञान 'शब्दब्रह्म' को अर्थात् वेद और उपनिषद् को पार कर जाता है, 'शब्दब्रह्मातिवर्तते।
vi. 44
जो भी हो, देखते हैं कि इस सब का अर्थ क्या है; क्योंकि इस विषय में तो हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि गीता जैसे समन्वयात्मक और उदार शास्त्र में आर्य-संस्कृति के इन महत्त्वपूर्ण अंगों का विचार केवल इन्हें अस्वीकार करने या इनका खंडन करने की दृष्टि से नहीं किया गया है।*...इसलिए चलते-चलते यहाँ पर यह गौर किया जा सकता है कि, वेद और उपनिषदों के मंत्र ही जिनके आधार हैं ऐसे इन नानाविध दार्शनिक संप्रदायों में जब इतना विरोध है तब गीता का यह कहना कि श्रुति बुद्धि को घबरा और चकरा देती है, उसे कई दिशाओं में घुमा देती है, 'श्रुतिविप्रतिपन्ना', कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज भी भारत के पंडितों और दार्शनिकों के बीच इन प्राचीन वचनों के अर्थों के संबंध में कितने बड़े-बड़े शास्त्रार्थ और झगड़े हो जाते हैं और वे सभी कितने विभिन्न निष्कर्षों तक पहुँचते हैं! इनसे बुद्धि खिन्न और उदासीन होकर, 'गन्तासि निर्वेदं', नवीन और प्राचीन शास्त्र वचनों को, 'श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च', सुनने से इन्कार कर के स्वयं ही गूढ़तर, आंतर और प्रत्यक्ष अनुभव के सहारे सत्य का अन्वेषण करने के लिये अपने अन्दर प्रवेश कर सकती है।
ⅱ.52 , ii.53
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।॥४७॥
४७. कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, परंतु केवल कर्म करने का, कर्मफल का कभी भी नहीं है; कर्मों के फलों को कमाँ का उद्देश्य न बना, अकर्म (कर्म परित्याग) में भी तेरी आसक्ति न हो।
कर्मफल तो अनन्य रूप से सभी कर्मों के स्वामी का ही है; हमारा इससे इतना ही प्रयोजन है कि सच्चे और सावधान कर्म के द्वारा उसका फल तैयार करें और यदि यह प्राप्त होता है तो इसे इसके दिव्य स्वामी को सौंप दें। तत्पश्चात् जैसे हमने फल के प्रति आसक्ति का त्याग किया है वैसे ही हमें कर्म के प्रति आसक्ति भी त्यागनी होगी। किसी भी क्षण हमें किसी काम, किसी कार्यक्रम या किसी कार्यक्षेत्र के स्थान पर दूसरे को ग्रहण करने अथवा, यदि प्रभु का स्पष्ट आदेश हो, तो सब कर्मों को छोड़ देने के लिये भी तैयार रहना होगा। अन्यथा हम कर्म प्रभु हितार्थ नहीं कर रहे होते, अपितु कर्म से मिलनेवाली निजी सन्तुष्टि एवं प्रसन्नता के लिये अथवा राजसिक प्रकृति को कर्म की आवश्यकता होने के कारण या अपनी रुचियों की पूर्ति के लिये कर रहे होते हैं; परंतु ये सब तो अहं के पड़ाव और अड्डे हैं।.... अन्त में, जैसे कर्मफल तथा कर्म के प्रति आसक्ति को हृदय से बाहर निकाल दिया गया है, वैसे ही अपने कर्त्ता होने के विचार तथा भाव के प्रति अन्तिम दृढ़ आसक्ति को भी छोड़ना होता है; भगवती शक्ति को अपने ऊपर तथा भीतर सच्ची तथा एकमात्र कर्नी के रूप में जानना एवं अनुभव करना होता है।
'कर्मण्येवाधिकारस्ते' यह एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और सामान्यतया इसी को गीता का परम वचन मान लिया जाता है। यहाँ श्रीअरविन्द ने इसका संकेत कर ही दिया है कि प्राणिक सत्ता कर्म के पीछे अपने निहित हेतु रखती है कि उससे उसे यह या वह अभीष्ट फल प्राप्त होगा जबकि भगवान् कह रहे हैं कि फल की आशा का परित्याग करके कर्म करो। परंतु सामान्य मनुष्य तो लाभ-अलाभ, सुख-दुःख आदि आधारों पर ही कर्म करता है और इनके बिना तो उसके कर्म का आधार ही नहीं रहेगा और वह कर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य के कर्म का आधार है कामना, अन्य तो उसके लिए कोई आधार ही नहीं है। गीता सबसे पहले मनुष्य की प्राण शक्ति के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास करती है क्योंकि उसकी अन्य सत्ताओं में वही सबसे अधिक प्रबल है। दूसरे श्लोक में भगवान् कहते हैं कि कर्मों के फलों को कमाँ का उद्देश्य न बना, अकर्म (कर्म परित्याग) में भी तेरी आसक्ति न हो।
-------------------------------------------
"गीता बाद के अध्यायों में वेदों और उपनिषदों की बड़ी भारी प्रशंसा करती है। वहाँ कहा गया है कि वे ईश्वर-प्रणीत शास्त्र हैं, शब्दब्रह्म हैं। स्वयं भगवान् ही वेदों के ज्ञाता और वेदांत के प्रणेता हैं, 'वेदविद् वेदान्तकृत'। सब वेदों के वे ही एकमात्र ज्ञातव्य विषय हैं, 'सर्वैः वेदैः अहमेव वेद्यः', इस भाषा का फलितार्थ यह होता है कि वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान का ग्रंथ और इन ग्रंथों के नाम इनके उपयुक्त ही हैं।
xv.15
अब यदि प्राणिक सत्ता को कर्म फल की चाह न दी जाए तब भी वह सूक्ष्म रूप से स्वयं उस कर्म में ही रस लेने लग जाती है और उसे ही ऊँचा कर्म बताने लगती है। इस बात में ही प्राण बहुत रस लेने लगता है कि उसे फल की परवाह नहीं है और गर्वित होकर कहता है कि वह लाभ-हानि नहीं देखता, वह तो तटस्थ है, श्रीमाताजी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पित है। इस प्रकार वह उसमें भी रस लेने लग जाता है। उसे तो जो कुछ भी मिलता है वह उसी में रस लेने लग जाता है। इसलिए गीता कहती है कि कर्म करने या न करने में भी रुचि न रखो, किसी कर्म के प्रति यदि आसक्ति है तो उसे तुरन्त ही छोड़ने के लिए तैयार रहो। इसके बाद, यह भाव कि मैं निष्काम कर्म करता हूँ, किसी वासना से नहीं करता, यह कर्त्तापन का अभिमान बना रहता है। इसलिए वास्तव में तो प्राण के सारे प्रसार पर, उसके इस प्रकार के व्यापार पर ही लगाम लगानी होगी, उसे बंद कर देना होगा। इसीलिये गीता में भगवान् तीसरे अध्याय में कहते हैं कि 'जो लोग समझते हैं कि वे स्वयं कर्मों के कर्ता हैं वे महामूर्ख हैं और यदि वे नहीं समझ पाते तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। परन्तु वास्तव में कर्म तो मेरे अधीन होकर मेरी प्रकृति ही करती है।' तब भी मनुष्य तो इन सब कर्मों को अपनी अहं चेतना के कारण स्वयं पर आरोपित करता है और फिर उनका प्राण कर्म के फल की इच्छा करता है। यहाँ गीता का सारा प्रयास एक ऐसा मानसिक अंकुश तैयार करने का है जिसमें प्राण की सब वृत्तियों के दरवाजे बंद कर दिये जाएँ, हालाँकि इस प्रयास में सफल होने की तो लगभग कोई संभावना ही नहीं है परंतु फिर भी कोई संरचना तो निर्मित करनी ही होगी जिसके सहारे व्यक्ति आगे बढ़ सके अन्यथा गीता आगे विकास करे ही कैसे। इसीलिए धीरे-धीरे ऐसी संरचनाएँ तैयार की जा रही हैं जिनके आधार पर बढ़ा जा सके और फिर यथासमय उन्हें उच्चतर ज्ञान के द्वारा अतिक्रम कर दिया जाए। केवल श्रीअरविन्द ने ही इस ओर ध्यान दिलाया है कि गीता का यह एक ऐसे निष्कर्ष तक ले जाने का तरीका है जहाँ यह समझ आ जाएगा कि समस्या का ऐसे किन्हीं भी तरीकों से समाधान नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि यही बात होती और इसी उपदेश से निष्काम कर्म साधित हो जाता तब तो फिर पूर्ण सिद्धि पहले ही सिद्ध हो जाती और इससे आगे गीता का उपदेश करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए, जब तक वर्तमान कर्म के हेतु की सारी जड़, अहं, को ही नहीं निकाल दिया जाता, जब तक दूसरों से पृथक् होने का बोध रहेगा, तब तक निष्काम कर्म संभव ही नहीं है। अवश्य ही, धीरे-धीरे यह सूक्ष्म होता जाता है, इसके रंग बदलते जाते हैं। परंतु ऐसा होने पर भी व्यक्ति साधना की संसिद्धि या फिर भगवान् की प्राप्ति की अपनी आसक्ति से तो ऊपर नहीं उठ सकता क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति का यही निहित हेतु है कि किस प्रकार उसे भगवान् की उपलब्धि हो जाए। परंतु यह सिद्ध हो जाए ऐसा संभव नहीं है और वर्तमान में गीता का यह उद्देश्य भी नहीं है। यह तो अर्जुन की तैयारी चल रही है, धीरे-धीरे उसे संवर्धित किया जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले अर्जुन को कहा गया है कि जय-पराजय को समान मानकर कर्म कर। पर अर्जुन पूछता है कि जब जय और पराजय मेरे लिए समान ही हों तो फिर कर्म करना ही क्यों चाहिये। इसीलिए गीता कहती है कि भगवान् की प्रसन्नता के निमित्त यज्ञ रूप से कर्म कर। हालाँकि यह नहीं है कि ऐसा कह देने भर से ही वह ऐसा कर्म कर सकता है, परंतु इस प्रकार एक मानसिक विचार तो आगे विकसित होता है। उदाहरण के लिये, यदि यह बोध रखकर हम कर्म करें कि कौनसा कर्म श्रीमाताजी को प्रसन्न करेगा और कौनसा नहीं तो इससे हम बहुत से कर्मों से बच सकते हैं। और जो कर्म करेंगे उनमें भद्देपन से, निम्न वृत्तियों आदि से कुछ हद तक बच जाएँगे। भगवान् की प्रसन्नता के निमित्त यज्ञ रूप से कर्म करना ऐसी चीज नहीं है जो सोचने मात्र से ही साधित हो जाए। यह यज्ञ का आरोहण तो जीवनपर्यंत का आरोहण है। सारा वेद इसी यज्ञ के विचार पर आधारित है कि एक बार जब यह भाव आ जाए कि समस्त क्रियाएँ आत्मा की प्रसन्नता के लिए की जानी चाहिये तब हमारी यात्रा भौतिक, प्राणिक तथा मानसिक स्तरों व उनके व्यवधानों से होकर लक्ष्य की ओर आगे चलने लगती है। हालाँकि तीसरे अध्याय में तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीता केवल बाहरी यज्ञ की ही बात कर रही है। परंतु चौथे अध्याय में भगवान् स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म ब्रह्म रूप हैं और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब वर्णन तो प्रतीकात्मक था जबकि गीता का वास्तविक लक्ष्य तो इससे भी महत्तर है। इस प्रकार गीता की सारी शिक्षा का आधार यहीं से निर्मित होना आरंभ हो गया है और हमें इसी परिप्रेक्ष्य में इसे समझना चाहिए। इस प्रकार सबसे पहले कर्मफल के प्रति आसक्ति के त्याग, फिर कर्मों के प्रति आसक्ति के त्याग और तत्पश्चात् कर्त्तापन के अभिमान के त्याग का प्रतिपादन कर के कम-से-कम हमारी बुद्धि को तो इस विषय पर स्पष्ट बोध प्रदान कर दिया गया है। और इस प्रश्न के उत्तर में कि ऐसा कर्म संभव ही कैसे है, यज्ञ-रूप कर्म की बात बता दी गई है कि सभी कर्मों को उत्तरोत्तर यज्ञ के रूप में किया जाना होगा।
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।।४८।।
४८. हे धनञ्जय! आसक्ति का परित्याग कर के, सफलता और असफलता में सम-भाव रखते हुए, योग में स्थित रहते हुए अपने समस्त कर्मों को कर; क्योंकि योग का अर्थ इस समता से ही है।
आत्मा, मन और हृदय में पूर्ण समता प्राप्त कर के हम अपनी उस सच्ची एकात्म्य आत्मा को अनुभव कर लेते हैं जो सभी सत्ताओं के साथ एकीभूत है, उसके साथ भी एकीभूत है जो अपने-आपको इन सब सत्ताओं में तथा उस सब में प्रकट करता है जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं। यह समता और एकता एक अनिवार्य दोहरी नींव है जो हमें दिव्य सत्ता, दिव्य चेतना और दिव्य कर्म के लिये स्थापित करनी होगी। यदि हम सबके साथ एकाकार नहीं हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम दिव्य नहीं हैं। सब वस्तुओं, घटनाओं और प्राणियों के प्रति आत्मिक समता रखे बिना हम दूसरों को आध्यात्मिक रूप से नहीं देख सकते, न हम उन्हें दिव्य रूप से जान सकते हैं और न उनके प्रति दिव्य रीति से सहानुभूति ही रख सकते हैं। एकमेव शाश्वत एवं अनन्त परम शक्ति सब पदार्थों और सब प्राणियों के प्रति 'सम' है, और क्योंकि वह 'सम' है, वह अपने कर्मों और अपनी शक्ति के सत्य के अनुसार और प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी के सत्य के अनुसार पूर्ण ज्ञान के साथ कार्य कर सकती है।
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।।४९।।
४९. हे धनञ्जय! बुद्धियोग की अपेक्षा (फलेच्छा से किये जानेवाले) कर्म निश्चय ही अत्यंत निकृष्ट हैं; इसलिये तू इस बुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की कामना कर (इसे प्राप्त कर), जो मनुष्य अपने कर्मों के फल को कर्म का उद्देश्य बनाते हैं वे दीन-हीन, अधम (कृपण) होते हैं।
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥५०।।
५०. जिसने अपनी बुद्धि को भगवान् के साथ युक्त कर दिया है वह इस द्वंद्वमय लोक में ही शुभ कर्म और अशुभ कर्म इन दोनों का परित्याग कर देता है; इसलिये योगस्थ होने के लिये प्रयत्न कर; योग कर्मों में कुशलता है।
गीता कहती है कि योग कर्मों में कुशलता है, और इस उक्ति से इस प्राचीन सद्ग्रंथ का अभिप्राय यह है कि मन और सत्ता का रूपांतर, जिसे इसने योग की संज्ञा दी है, अपने साथ एक परिपूर्ण आंतरिक अवस्था तथा योग्यता लाता है जिसमें से कर्म का सही विधान और कर्मों का सही आध्यात्मिक और दिव्य फल या परिणाम उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार अपने बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। निश्चय ही इसका यह अर्थ नहीं था कि कोई चतुर सेनानायक या राजनेता या वकील या मोची योगी के नाम का अधिकारी है, इसका यह अभिप्राय नहीं था कि कर्मों में किसी भी प्रकार की कुशलता योग थी, अपितु योग से यह वैश्व समत्व तथा भगवदैक्य की एक आध्यात्मिक अवस्था द्योतित करती थी और योगस्थ कार्यकर्ता की कुशलता से इसका अभिप्राय दिव्य और वैश्व प्रकृति - जो कि अहंकार के बंधनों से तथा ऐंद्रिय-मन की सीमाओं से मुक्त हो - की लय के प्रति आत्मा और उसके उपकरणों की पूर्ण अनुकूलनता से था।
...योगस्थ होकर किया जाने वाला कर्म न केवल उच्चतम अपितु अत्यंत ज्ञानपूर्ण, सांसारिक विषयों के लिये भी अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत अमोघ होता है...
इसमें प्रश्न यह उठता है कि आखिर समता हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इसे हम एक रूपक के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि भगवान् की अभिव्यक्ति के लिए हम मिलकर कोई नाटक कर रहे हैं और उसमें सबकी भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ हैं। अब यदि इसमें कोई कुछ दृश्यों को अच्छा और कुछ दृश्यों को बुरा समझकर प्रभावित होता हो तो फिर वह अपना संवाद सही ढंग से नहीं बोल पाएगा और अपनी भूमिका को अच्छी तरह नहीं निभा पाएगा। अतः उच्चतर चेतना में होने पर ही व्यक्ति में सच्ची समता आती है। जब हम इस नाटक की पटकथा समझ जाएँगे और यह समझ जाएँगे कि यह वास्तव में एक नाटक है और इसमें हम सभी अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं तब ऐसा जानकर हम विचलित नहीं होंगे। इसलिए ब्रह्म चेतना से जुड़ने पर ही सच्ची समता आती है। अर्थात् जब हमें इन सारी बातों का ज्ञान हो जाएगा तभी समता आ सकती है, इससे पहले नहीं। फिर हम जान जाते हैं कि हम सब एक ही हैं और हमारा एक उद्देश्य है जिसमें हम सब लोग मिलकर भाग ले रहे हैं इसलिए हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अतः समता आवश्यक है। समझने के लिए यह एक दृष्टिकोण है। यही बात गुणों की थी और यही बात समता की है। यदि हम बाहरी प्रतीति से प्रभावित होते हैं तो हम समुचित कर्म नहीं कर सकते। परन्तु जिस प्रकार हमारा क्रमविकास हुआ है उस गठन के कारण हम प्रभावित होते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक सत्य को पाने के लिए हमें उस स्तर तक जाना आवश्यक है जहाँ हम ब्रह्म चेतना को प्राप्त कर सकें। 'समत्वं योग उच्यते', समता ही योग है। क्योंकि योग होगा तभी समता आएगी। इसके बिना समता नहीं आ सकती। तो यह तो हुई समता की बात।
दूसरा है, 'योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात् योग ही कर्मों में कुशलता है न कि कर्मों में कुशलता योग है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हो तो बहुत कुशल परंतु बिना यह प्रश्न पूछे ही चल पड़े कि उसे जाना कहाँ है तो उसकी कुशलता का लाभ ही क्या हुआ। योग ही वह सही दिशानिर्देश दे सकता है। योग ही व्यक्ति को बतलाएगा कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। इसलिए सच्ची कुशलता तो कर्म में योगयुक्त होने में ही है अन्यथा हमारे कर्म अकुशल हैं, क्योंकि योगयुक्त हुए बिना तो कर्मों का केंद्र अहं ही होगा जिससे कि कोई भी काम पूरी कुशलता के साथ किया ही नहीं जा सकता। इसलिए योग-युक्त होना ही सभी चीजों में सच्ची कुशलता लाता है।
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ।।५१।।
५१. जिन ज्ञानी मनुष्यों ने अपनी बुद्धि को भगवान् के साथ युक्त कर दिया है वे कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर देते हैं और जन्मरूप बंधन से मुक्त होकर वे दुःख-दर्द से परे उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।
परन्तु जीवन की ओर अभिलक्षित समस्त कर्म योगी को उसके व्यापक ध्येय से दूर ले जाता है क्योंकि सर्वमान्य रूप से यह ध्येय इस दुःख-शोकमय मानव-जन्म के बन्धन से छुटकारा पाना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है... जो योगी कर्मफल की इच्छा के बिना, भगवान् के साथ योग में युक्त होकर कर्म करते हैं, वे जन्म-बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस परम्-पद को प्राप्त होते हैं, जहाँ दुःखी मानव जाति के मन और प्राण को सताने वाली कोई भी व्याधि नहीं होती।
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥
५२. जब तेरी बुद्धि मोहजाल को पार कर जाएगी तब तू शाख के उन वचनों के प्रति, जो तूने सुने हैं या सुनने शेष हैं, उदासीन हो जाएगा।
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।।५३ ।।
५३. जब श्रुति से किंकर्तव्यविमूढ़ हुई तेरी बुद्धि समाधि में निश्चल और स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त करेगा।
...शास्त्र का शब्द बंधनकारी और भरमानेवाला होता है, जैसा कि ईसाइयत के दूत (ईसा) ने अपने अनुयायियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि 'शब्द मारता है जबकि उसका भाव या मर्म है जो तारता है और एक सीमा है जिसके परे शाखों की भी कोई उपयोगिता नहीं रहती। ज्ञान का वास्तविक स्रोत है हृदय में विराजमान ईश्वर; गीता में भगवान् कहते हैं कि "मैं (ईश्वर) प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही ज्ञान निःसृत होता है।" शाख तो उस आंतर वेद (ज्ञान) का, उस स्वयंप्रकाश सत्-तत्त्व का केवल शब्दमय विग्रह है, यह शब्द-ब्रह्म हैः वेद कहता है, मंत्र हृदय से निकला है, उस गुह्य स्थान से जो सत्य का सदन है, 'सदनाद् ऋतस्य, गुहायां'। वेद का यह मूलस्रोत ही उसका प्रमाण है; फिर भी वह अनंत सत्य अपने शब्द की अपेक्षा महत्तर है। और तुम किसी भी सद्ग्रंथ के विषय में ऐसा नहीं कह सकते कि वही एकमात्र सर्वथा-पर्याप्त है, इसके अतिरिक्त और कोई सत्य ग्राह्य नहीं हो सकता, जैसा कि वेद के विषय में वेदवादी कहते थे, 'नान्यदस्तीतिवादिनः'। यह बात (अनेक भ्रमादि से) रक्षा vec 4h * 7 वाली और मुक्तिदायी है, और संसार के सभी सद्ग्रंथों के विषय में कही जा सकती है। बाइबल, कुरान, चीन के धर्मग्रंथ, वेद, उपनिषद्, पुराण, तंत्र, शास्त्र और स्वयं गीता आदि सभी वर्तमान में विद्यमान या किसी समय विद्यमान रहे सद्ग्रंथ हैं, उन सबमें जो सत्य है उसे तथा जितने तत्त्ववेत्ता, साधु-संत, ईश्वरदूत और अवतारों की वाणियाँ हैं, उन सबको एकत्र कर लें तो भी आप यह न कह सकेंगे कि जो कुछ है बस यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं या जिस सत्य को आपकी बुद्धि इनके अन्दर नहीं देख पाती वह सत्य ही नहीं, क्योंकि वह इनके अन्दर नहीं मिलता। यह तो सांप्रदायिकों की संकीर्ण बुद्धि हुई या फिर सब धर्मों से अच्छी-अच्छी बात चुननेवाले धार्मिक मनुष्य की मिश्रित बुद्धि हुई, स्वतंत्र और प्रकाशमान मन का और ईश्वरानुभवप्राप्त जीव का अबाधित या मुक्त सत्यान्वेषण नहीं। पहले श्रुत हो या अश्रुत, वह ही सदा सत्य है जिसको मनुष्य अपने हृदय की ज्योतिर्मय गहराइयों में देखता या अखिल ज्ञान के स्वामी सनातन वेदविद् सर्वज्ञ परमेश्वर से अपने हद्देश में श्रवण करता है।
xv 15
अब यह एक गहरा सूत्र बता दिया गया है कि जिस सत्य को हम अपने हृदय में देखते हैं उसके बारे में पहले किसी ने बताया है या नहीं बताया है, वेद, उपनिषद् या अन्य कोई उसके पक्ष में बोलता है या विपक्ष में, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि हृदय में विराजमान सत्य तो सदा ही सत्य है। और भगवान् की लीला का कोई अंत नहीं है। आज तक किसी ने 'उनके' बारे में जो कुछ भी बताया है वे तो केवल प्रारम्भिक बातें ही हैं क्योंकि सत्य का कोई अंत नहीं है। यह इस तरह की चीज है जिसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और वेद, उपनिषद् आदि ग्रन्थों को विद्वानों और मनीषियों ने अपने अनुभव के आधार पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अभिव्यक्त किया है, इसलिये ये बहुत ही अच्छे हैं। और उनका अनुभव बहुत ही विशाल और बहुत ही गहरे स्तर से है इसलिए वह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पर जहाँ तक हृदय में विराजमान इस सत्य की बात है, तो इसके सामने उनका कुछ मूल्य नहीं है। इसीलिये कहा गया है कि जिसे ज्ञान हो गया है उसके लिए सारे वेदों का उतना ही अर्थ रह जाता है जितना कि चारों ओर बारिश और बाढ़ की स्थिति में कुएँ के पानी का रह जाता है। परंतु हमारे अनुभव का उतना ही मूल्य है जितना हमारा हृदय पवित्र है, अन्यथा तो वह विकृत हो सकता है। अपने-आप में उस अनुभव में कमी नहीं है, अनुभव तो बिल्कुल सही है, परन्तु हमारे द्वारा उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो जाएगी। यदि हमारे दर्पण का केंद्र-बिन्दु सही नहीं है तो हम अनुभव का सही अर्थ लगा ही नहीं सकेंगे। व्यक्ति अपने हृदय में जो देखता है, अंततः तो वही सत्य है, तथा अन्य किसी सत्य का हमारे लिए कोई मूल्य भी नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति रात-दिन किसी ज्योति को देख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति आस्तिक है या नास्तिक, परंतु यदि कोई दूसरा व्यक्ति यह कहे कि जो वह अनुभव कर रहा है वह सत्य नहीं है तो उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो श्रीअरविन्द ने कुछ यों कहा कि, 'मैं स्वयं भी नास्तिक था, परंतु जब स्वयं भगवान् ही मेरे पास चले आए और कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं हूँ, तो फिर कैसे मैं उनकी सत्ता को नकार दूँ, भले लोग कुछ भी क्यों न कहते हों।' (CWSA 12 : 424)
इसी तरह की बात श्रीअरविन्द यहाँ बता रहे हैं कि सारे उपनिषद्, गीता, बाइबल, पुराण आदि जितने भी ग्रंथ हैं उनमें हुई अभिव्यक्ति भी भगवान् के सत्स्वरूप को सीमित नहीं कर सकती। क्योंकि कब व किस समय और किस क्षेत्र में वे क्या कर दें इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चाहे व्यक्ति को कितने भी विशाल और उच्च अनुभव क्यों न प्राप्त हो जाएँ, परंतु उनके बाद भी किसी भी क्षण उसे एक ऐसा अप्रत्याशित अनुभव प्राप्त हो सकता है जो उसके पूर्व के अनुभवों को सर्वथा अतिक्रम कर सकता है। और यह कोई असामान्य नहीं अपितु सदा ही होने वाली घटना है। इससे हमें यह आभास होता है कि अपने-आप में वह परम तत्त्व कितना अनंत और विशिष्ट है जो सदा ही नित-नूतन बना रहता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को यदि कोई अनुभव हो गया हो तो उसी को अंतिम मानकर उसके आधार पर वह भगवान् के विषय में अपनी मानसिक रचनाएँ तैयार कर सकता है। 'वह' तो ऐसा तत्त्व है जो अचिंत्य है। सदा ही 'वह' व्यक्ति के अनुभव में इस रूप में आता है कि व्यक्ति को बहुत ही अचंभा होता है कि यह क्या है। इस प्रकार धीरे-धीरे बहुत सारे अचंभों में से गुजरने पर व्यक्ति को कुछ थोड़ा-सा अधिक गहरा आभास प्राप्त होता है। परंतु वह भी केवल एक दृष्टिकोण मात्र ही होता है, और उससे 'वह' सीमित नहीं हो जाता। परन्तु फिर भी वह अनुभव अपने आप में सत्य है, कारगर है। इस तरह की बात का श्रीअरविन्द ने गीता में वर्णन किया है।
अर्जुन उवाच
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ॥५४।।
५४. अर्जुन ने कहाः हे केशव! जो मनुष्य समाधि में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थित हो गयी है उसका क्या लक्षण होता है? स्थितबुद्धि साधु किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार चलता है?
अर्जुन औसत मनुष्य के मन में उठनेवाले प्रश्न को प्रकट करते हुए इस महान् समाधि के कुछ बाह्य, शारीरिक और व्यावहारिक रूप में पहचाने जा सकने योग्य लक्षणों के विषय में पूछता है... इस तरह के कोई लक्षण नहीं बताये जा सकते और न श्रीगुरु बतलाने का प्रयास ही करते हैं; क्योंकि समाधि की केवल कोई संभवनीय कसौटी आंतरिक ही है और उसे लागू करने के लिए विरोधी मनोगत शक्तियाँ बहुत हैं। मुक्त पुरुष का महान् लक्षण समता है और समता की पहचान के लिये जो अति स्पष्ट चिह्न हैं वे भी आंतरिक हैं।
श्रीभगवान् उवाच
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।।५५।।
५५. श्रीभगवान् ने कहाः हे पार्थ! जब मनुष्य मन में रहने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है।
समाधिस्थ मनुष्य का लक्षण यह नहीं है कि वह पदार्थों और परिवेश का तथा अपने मन और देह का संज्ञान ही खो बैठता है और उसके शरीर को जलाने या पीड़ित करने पर भी उसे इस चेतना में लौटाया न जा सके, जैसा कि साधारणतया लोग समाधि द्वारा समझते हैं; इस प्रकार की समाधि तो चेतना की एक विशिष्ट प्रकार की प्रगाढ़ता है, यह इसका कोई मूल लक्षण नहीं है। समाधि की कसौटी है सब कामनाओं का बहिष्कार, किसी भी कामना का मन तक न पहुँच सकना, और आन्तरिक अवस्था से ही यह स्वतंत्रता उत्पन्न होती है, जिसमें आत्मा का आनन्द अपने ही भीतर केंद्रीभूत रहता है, साथ ही मन सम, स्थिर तथा आकर्षणों और विकर्षणों से तथा बाह्य जीवन के धूप, आँधी तथा तनाव आदि फेर-बदलों से परे उच्चासीन रहता है। बाह्य रूप hat H क्रिया करते हुए भी यह भीतर की ओर ही आकृष्ट रहता है; बाह्य पदार्थों को देखते हुए भी यह आत्मा में ही एकाग्र रहता है; दूसरों की दृष्टि में सांसारिक काम काज में व्यस्त और तल्लीन होने पर भी वह सर्वथा भगवान् की ओर लगा रहता है।
समता का पता तो बाहरी घटनाओं के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया से ही चल जाएगा। जिसे व्यक्ति अपनी प्रिय चीजें बताता है उनके साथ यदि कुछ दुःखद घटित होता है तब समता है या नहीं इसका पता लग जाता है। यदि जिससे व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं उसके साथ कुछ अप्रिय घटित होता है और व्यक्ति अप्रभावित रहे तो इससे समता का पता नहीं लग सकता। पर यदि प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, घर में आग लग जाए या अन्य कुछ दुःखद या अप्रिय घटित हो जाए और तब भी व्यक्ति विचलित न हो तो हम सोचते हैं कि ऐसी मनोदशा के लिए उसे कितना अभ्यास करना पड़ा होगा, क्योंकि हमारा जिस प्रकार का वर्तमान गठन है उसमें यही कर पाना हमारे लिए तो एक महत् कार्य होता है। इसके परे तो हम और कोई बात सोच ही नहीं सकते। परंतु समत्व की स्थिति तो एक ऐसी सहज-सिद्ध स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति एक ऐसी चेतना में प्रतिष्ठित होता है जहाँ इन बातों का उसके लिए कोई महत्त्व ही नहीं होता। जैसे कि यदि किसी सड़क पर बहुत सारे फूल-पत्ते बिखरे हों और यदि वे हवा से इधर-उधर हो जाएँ या फिर नष्ट भी हो जाएँ तो व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता क्योंकि इन चीजों का उसके लिए कोई महत्त्व ही नहीं होता। जब व्यक्ति को परमात्मा का अनुभव हो जाता है तब उसके लिए अन्य चीजों का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता, वे चाहे इधर जाएँ या उधर जाएँ, क्योंकि व्यक्ति सम-स्थिति में होता है और सम इसलिए होता है क्योंकि उसका इन घटनाओं से वास्तव में कुछ बनने-बिगड़ने वाला नहीं है। व्यक्ति को ऐसी चीज प्राप्त हो चुकी होती है जिसके सामने दुनिया में जो कुछ भी है या नहीं है, दुनिया जो दे सकती है या नहीं दे सकती, उस सबकी कुछ भी कीमत नहीं रह जाती। इसलिए ऐसे में समता तो अपने-आप ही आ जाती है।
इससे भी अधिक सच्ची समता तब आती है जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अब जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वही चित्रकार है तो उसके भिन्न-भिन्न रंग किसी दूसरे को तो सौभाग्य-दुर्भाग्य प्रतीत हो सकते हैं परंतु स्वयं उसे तो वे चित्र के अनुरूप स्वाभाविक ही प्रतीत होंगे। इसी तरह, शरीर के आने या जाने पर सामान्यतः हम विचलित होते हैं, परंतु जिसे यह ज्ञान हो गया है कि यह तो अपने पुराने कपड़े बदलने जैसी ही क्रिया है वह व्यक्ति उससे विचलित नहीं हो सकता। क्योंकि वह जानता है कि ये सब चीजें भगवान् को अभिव्यक्त करने के लिए ही इतनी सारी घटनाएँ मात्र हैं। जैसे कि जब नाटक की पूरी रूपरेखा व्यक्ति को पता हो तो वह उसे बखूबी निभाता अवश्य है परंतु किन्हीं दृश्यों से वास्तव में डर नहीं जाता या विचलित नहीं हो जाता। इसलिए जब व्यक्ति को कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाती है जिसके सामने अन्य सभी चीजों का कोई वास्तविक मूल्य ही नहीं रह जाता तब फिर वह और अधिक विचलित नहीं होता।
परंतु जब मनुष्य धन-संपत्ति, सुख, आत्म-संतुष्टि आदि चीजों में लिप्त रहता है, तो यह एक बड़ी भयंकर और दयनीय स्थिति है। व्यक्ति के अन्दर अनन्त खजाने निहित हैं। यदि एक बार वह उन्हें थोड़ा-सा भी देख ले तब फिर इन सब बाहरी चीजों का उसके लिए कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता और वह सच्चे रूप से अपने कर्म कर सकता है क्योंकि तब उसके बाहरी परिणाम के प्रति वह अप्रभावित रहता है, इसलिए उसके लिए तो सब अच्छा ही होता है। अतः अपने भीतर वह आनन्द का अनुभव करता है। तब फिर व्यक्ति को सृष्टि की बाहरी घटनाओं से कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि सभी कुछ केवल आत्म-अभिव्यक्ति का यंत्र बन जाता है। इसलिए जब सच्चे अनुभव के अंदर आनन्द का स्रोत खुल जाता है तब फिर कोई समस्या नहीं रहती, और समता अपने-आप ही स्थापित हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि तब व्यक्ति बाहरी चीजों के प्रति लापरवाह हो जाता हो, बल्कि वह सही दृष्टिकोण से अपनी भूमिका निभा सकता है। यह देखने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है।
प्रश्न : हम कह रहे हैं कि अपने हृदय का सत्य ही सर्वोपरि है। जब वेद में सभी मूलभूत सत्य और सभी मूलभूत अनुभव समाहित हैं तो हमारे हृदय के अनुभव के साथ वेद में निहित अनुभवों का कोई विरोध तो नहीं होना चाहिये?
उत्तर : स्वयं वेदों की वाणी तो सही है, उसमें तो पूर्ण सत्य है। पर व्यक्ति का मन, उसकी बुद्धि उसका जो अर्थ लगाते हैं वह संदिग्ध हो सकता है। वे इसका दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने जो समझा है वही सत्य है। क्योंकि वेदों का सत्य तो यथार्थ और प्रामाणिक है। योगी श्री कृष्णप्रेम कहते हैं कि अनुभव पर संदेह नहीं किया जा सकता, हालाँकि, उसकी मानसिक अभिव्यक्ति पर अवश्य संदेह किया जा सकता है। व्यक्ति उस अनुभव का क्या अर्थ लगाता है उस पर संशय किया जा सकता है। उसमें तो सदा ही सुधार की संभावना रहती है। जैसे कि यदि व्यक्ति को श्रीमाताजी का अनुभव हो और पूरी सत्ता आनंद से भर जाए तो इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। सारा वेद भी यदि इसका खण्डन करे तो भी उसका कोई महत्त्व नहीं है। व्यक्ति उसका अर्थ क्या लगाता है, वह एक दूसरी बात है। परंतु स्वयं उस अनुभव पर संदेह नहीं किया जा सकता।
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः स्थितघीर्मुनिरुच्यते ।।५६।।
५६. दुःखों में जिसका मन व्याकुल नहीं होता और सुखों में (उनसे भोगजन्य सुख लेने की) कामना से रहित होता है, जिससे राग, भय और क्रोध दूर हो गये हैं, वह स्थितप्रज्ञ मुनि है।
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।५७।।
५७. जो चाहे शुभ प्राप्त हो या अशुभ सभी में अनुरागरहित रहता है, शुभ के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अशुभ से घृणा नहीं करता उसकी बुद्धि ज्ञान में दृढ़प्रतिष्ठ होती है।
यदा संहरते चायं कूर्मो ऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।५८ ।।
५८. कछुआ जैसे अपने अंगों को अपने खोल में खींच लेता है, इस ही प्रकार जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को इन्द्रियों के विषय से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि दृढ़प्रतिष्ठ होती है।
.....बुद्धि की क्रिया की दो सम्भावनाएँ हैं। या तो वह अपना निम्नगामी और बहिर्मुख रुख अपना कर प्रकृति के तीनों गुणों की लीला में इन्द्रियानुभवों और संकल्प की छितरी हुई क्रियाओं में संलग्न रह सकती है, या यह अपना ऊर्ध्वगामी और अंतर्मुख रुख अपनाकर, अब और अधिक प्रकृति के विकर्षणों के अधीन न रहकर, प्रशांत सचेतन आत्मा की स्थिरता और अविकार अडिग विशुद्धता में चिरशांति और समता की ओर गति कर सकती है। पहले विकल्प में आत्मनिष्ठ आंतरिक सत्ता इन्द्रियों के विषयों के अधीन रहती है, वह वस्तुओं के बाह्य संपर्क में ही निवास करती है।... अतः, स्थिर एकाग्रता तथा अध्यवसाय के साथ हमें बुद्धि की ऊर्ध्वमुख और अंतर्मुख अभिमुखता को हो दृढ़प्रतिष्ठ भाव, व्यवसाय, से अपनाना होगा; हमें इसे दृढ़तापूर्वक पुरुष के प्रशांत आत्मज्ञान में स्थित करना होगा। इसमें निःसंदेह ही सबसे पहली गति होनी चाहिए कामना से छुटकारा पाना जो कि दुःखों और कष्टों का संपूर्ण मूल है; और कामना से छुटकारा पाने के लिये कामना के मूलकारण का, अर्थात् विषयों को पाने और भोगने के लिए इन्द्रियों के बहिर्गमन का, अंत करना होगा। जब वे इस प्रकार बाहर दौड़ पड़ने में प्रवृत्त हों तब उन्हें पीछे खींचना होगा, उन्हें उनके विषयों से हटा लेना होगा, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल के अन्दर खींच लेता है, वैसे ही इन्द्रियों को उनके मूल स्रोत मन में लाकर शांत करना होगा, और मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा एवं उसके आत्मज्ञान में लाकर शांत करना होगा जो कि प्रकृति के कर्म को देखता है, उसमें फँसता नहीं; क्योंकि ऐसी किसी चीज की वह कामना नहीं करता जो विषयाश्रित जीवन प्रदान कर सकता है।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
रसवर्णं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ।।५९।।
५९. विषयों का परित्याग कर देने वाले देही (मनुष्य) के इन्द्रियों के विषय तो दूर हो जाते हैं किंतु स्वयं विषयों में अनुराग, रस, बचा रहता है; परमात्मा के दर्शन कर लेने पर रस भी दूर हो जाता है।
यहाँ किसी प्रकार की भ्रांति न उठ पाए उससे बचने के लिए तत्क्षण ही श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं किसी बाह्य वैराग्य या विषयों के भौतिक संन्यास की शिक्षा नहीं दे रहा। आत्मानुशासन या संयम आदि से मेरा अभिप्राय सांख्यों के संन्यास या कठोर तपस्वियों के उपवासादि तप, कायाक्लेश या भोजन के त्याग की भी चेष्टा से नहीं है, क्योंकि मैं तो एक आंतरिक वैराग्य, कामना के परित्याग की बात कहता हूँ। देहात्म शरीरधारी को अपनी देह को नित्य दैहिक कर्म करने के योग्य बनाए रखने के लिये आहार देना होता है; निराहार होने से देही विषयों के साथ अपने दैहिक संबंध को हटा देता है परंतु इससे उस आत्मनिष्ठ संबंध से पीछा नहीं छूटता जो उस संपर्क को दुःखद बनाता है। उसमें विषयों का रस - रागऔर द्वेष जिसके दो पहलू हैं तो बना ही रहता है। इसके विपरीत देही को, अवश्य ही राग-द्वेष से अलिप्त आंतरिक रूप से बिना कोई कष्ट उठाए बाह्य स्पर्श को सह सकने में समर्थ होना चाहिए। अन्यथा विषय की तो निवृत्ति हो जाती है, 'विषया विनिवर्त्तन्ते', परन्तु आंतरिक निवृत्ति नहीं होती, मन की निवृत्ति नहीं होती; और इन्द्रियाँ मन की (आश्रित) हैं, आत्मनिष्ठ हैं, इसलिए रस की आंतरिक (आत्मनिष्ठ) निवृत्ति हो प्रभुता का एकमात्र वास्तविक लक्षण है। परन्तु विषयों से इस प्रकार का
निष्काम संपर्क, इन्द्रियों का इस प्रकार निर्लिप्त प्रयोग कैसे संभव है? यह संभव है परम् के दर्शन से 'परं दृष्टा'' -परम अर्थात् आत्मा, पुरुष - और बुद्धियोग के द्वारा उसके साथ संपूर्ण आत्मनिष्ठ सत्ता में युक्त होने से, एकत्व को प्राप्त होने से; क्योंकि वह 'एकनिष्ठ' आत्मा शांत है, अपने ही आनंद से संतुष्ट है, और एक बार यदि हमने अपने अन्दर रहनेवाले इस परम् पुरुष का दर्शन कर लिया और अपने मन और संकल्प को उसके ऊपर स्थापित कर दिया तो यह द्वन्द्वशून्य आनन्द, इन्द्रियों के विषयों से पैदा होनेवाले मानसिक सुख और दुःख का स्थान ग्रहण कर सकता है। यही मुक्ति का सच्चा तरीका है।
यदि इंद्रियों को कामनाओं की तृप्ति की ओर खुली छूट दी जाती रहेगी तो कामनाएँ कभी समाप्त नहीं होंगी, और यदि इंद्रियों पर निग्रह, या उनका दमन कर भी लिया जाए तो भी मन में तो उनके प्रति लिप्तता होती है इसलिए वह शांत नहीं होगा, और इस कारण उनकी तृप्ति की ओर सदा ही दबाव बना रहेगा जिससे लड़ते-लड़ते व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाएगी। यह है निग्रह और संयम में अन्तर। निग्रह का अर्थ है कि उन कार्यों का हठपूर्वक दमन करना जबकि संयम का अर्थ है कि न तो उन कार्यों को करना ही, बल्कि उनके विषय में कोई विचार तक नहीं आने देना। क्योंकि यदि मन में उसका विचार तो आए पर हम उसकी तृप्ति का दमन करें तो अन्दर ही अन्दर एक संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और हमारी शक्ति क्षीण होने लगेगी। इसीलिए गीता संयम को श्रेष्ठ बताती है।
हालाँकि, जब श्रीमाताजी से पूछा गया कि संयम कैसे प्राप्त करें तो श्रीमाताजी ने निग्रह करने के द्वारा ही उस तक पहुँचने का रास्ता बताया। निग्रह को पूरे बल के साथ स्थापित करो, पर उसी पर मत रुको, तब फिर संयम भी आ जायेगा। गीता के अनुसार संयम तब आता है जब हम परम् प्रभु को देख लेते हैं, और फिर केवल देखने की ही बात नहीं, व्यक्ति को उसमें आनन्द आने लगता है। उस आनन्द के सामने अन्य सभी निम्नतर सुख तुच्छ प्रतीत होते हैं। तब फिर व्यक्ति केवल भगवान् के कार्य हेतु ही शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन आदि तथा अन्य सब क्रियाएँ करता है, अंतर में प्रभु का जो स्पर्श है उसकी अभिव्यक्ति के लिए वह ये सब कार्य करता है, अन्यथा उसे इन कामों में कोई रुचि नहीं रह जाती और फिर वह इन्द्रियों के सुख के साधन के रूप में उन्हें उपयोग में नहीं लेता। अभी तो हम इन्द्रियों को सुख के साधन के रूप में काम में लेते हैं जबकि इनमें अपने आप में सुख की कोई संभावना ही नहीं है, बल्कि इनकी तुष्टि तो बाद ये व्यक्ति के मुँह में बुरा स्वाद छोड़ती हैं।
श्रीमाताजी कहती हैं कि सामान्य क्रम तो यह है कि पहले मन से उस कामना को निकाल दें और फिर उस कामना के वशीभूत हो कर्म भी न करें। परंतु यह तरीका अधिकांशतः सफल नहीं हो पाता। क्योंकि ऐसी प्राणिक शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति को इन चीजों को करने के लिए बाध्य करेंगी। परंतु जब उनके प्रलोभनों के बाद भी उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाता तब फिर धीरे-धीरे वे उसमें अपनी रुचि छोड़ देती हैं, और उसके पीछे अपना समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करतीं। यह एक मनोवैज्ञानिक अनुभव की बात है। हालाँकि यह काम है बहुत कठिन। श्रीमाँ ने यह एक तरीका बताया है, इसके अलावा और तरीके भी हो सकते हैं। परन्तु यहाँ सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियों को अपने तरीके से काम करने देता है तो उनकी पकड़ उस पर बढ़ती जाएगी, इसलिए इनकी निरंकुश क्रीड़ा को रोकना ही होगा। अतः प्रथम आवश्यकता है कि इंद्रियों के वशीभूत होकर कर्म करें ही नहीं।
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ।॥६०॥
६०. हे कौन्तेय! आत्मसंयम के लिये सच्चे हृदय से प्रयत्न करने वाले ज्ञानी, विवेकी पुरुष के भी मन को उग्र हठवाली इन्द्रियाँ बलपूर्वक हर लेती हैं।
निश्चय ही आत्म-संयम, आत्म-नियंत्रण कभी सरल नहीं होता। सभी बुद्धिमान मनुष्य इस बात को जानते हैं कि उन्हें थोड़ा-बहुत संयम करना चाहिए, अपनी इन्द्रियों को वश में करने की सलाह से अधिक सामान्य और कोई चीज नहीं है; परन्तु सामान्यतः यह उपदेश अपूर्ण रूप से ही दिया जाता है और इसका पालन भी अपूर्ण रूप से और वह भी बहुत ही सीमित और अपर्याप्त मात्रा में किया जाता है। फिर भी, पूर्ण आत्म-प्रभुत्व की प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम करनेवाला ज्ञानी, स्पष्टदृष्टि-संपन्न, बुद्धिमान् और विवेकी पुरुष भी अपने-आप को इन्द्रियों द्वारा वशवर्ती कर के बहा लिया गया पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन स्वभावतः ही अपने को इन्द्रियों के वशीभूत कर देता है, वह आंतरिक रस के साथ इन्द्रिय-विषयों को देखता है, उनका चिंतन या विचार करता है और उनको बुद्धि के लिए विचारों की व्यस्तता का और संकल्प के लिये तीव्र रुचि का विषय बना लेता है।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१।।
६१. उन समस्त इन्द्रियों को संयत कर के, मत्परायण होकर योग में दृढ़तापूर्वक स्थित हो; क्योंकि जिसकी इंद्रियाँ वशीभूत होती हैं उसकी शांत और विवेकशील बुद्धि अपने उचित स्थान पर दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित होती है।
इसलिए ऐसा न होने देना चाहिए और सब इन्द्रियों को पूरी तरह वश में ले आना चाहिए, क्योंकि इन्द्रियों के पूर्ण संयम से ही विज्ञ और स्थिर बुद्धि अपने स्थान में दृढ़प्रतिष्ठ हो सकती है।
केवल बुद्धि के अपने प्रयत्न से ही, केवल एक मानसिक संयम से ही यह कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकता; यह केवल ऐसी वस्तु के साथ युक्त होने से ही हो सकता है जो बुद्धि से ऊँची हो और स्थिरता तथा आत्म-प्रभुता जिसमें स्वभावसिद्ध हो। यह योग अपनी सफलता तक केवल समस्त सत्ता को भगवान् के प्रति - श्रीकृष्ण कहते हैं 'मेरी ओर, मत्परः' - निवेदित करने, उत्सर्ग करने और समर्पित करने से ही पहुँच सकता है; क्योंकि 'मुक्तिदाता' श्रीभगवान् हमारे अन्दर हैं, परंतु वे हमारा मन या हमारी बुद्धि या हमारी अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं हैं, ये तो केवल उपकरण हैं। हमें, जैसा कि गीता के अंत में बताया गया है, सर्वभाव से ईश्वर की ही शरण में जाना होगा। और इसके लिए पहले उन्हें अपनी संपूर्ण सत्ता का ध्येय बनाना होगा और उनसे आत्म-संबंध बनाये रखना होगा। 'सर्वथा मत्परायण होकर, मुझमें योगयुक्त होकर स्थित रह' इस अंश का यही अभिप्राय है। पर अभी यह अत्यंत क्षीण संकेतमात्र है, जो गीता की प्रतिपादनशैली के अनुरूप ही है। 'युक्त आसीत मत्परः' इन तीन शब्दों में वह परम रहस्य बीज-रूप से भर दिया गया है जिसका विस्तार आगे होना है।
ये तीन शब्द ही अंतिम चीज हैं और सारी समस्याओं का समाधान भी हैं। इन्द्रियाँ अच्छे से अच्छे व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती हैं और वह भी कुछ नहीं कर पाता। हम मन को बुद्धि के दृष्टिकोण से संयम करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु बुद्धि भी अपने-आप में सशक्त नहीं है। इन्द्रियों को संयम करने के लिए एक ऐसी चीज से जुड़ना होगा जो सहज रूप से इन सब चीजों से ऊपर है। परंतु उसके साथ युक्त होना हमारे लिए सहज नहीं है। परमात्मा की कृपा से तो यह तत्काल सिद्ध हो सकता है अन्यथा उसके लिए हमें प्रयत्न ही करना होगा। इसके लिए एक ही सूत्र है – 'युक्त आसीत मत्परः' - मेरे परायण होकर, मेरे से जुड़कर कर्म करो। ये चीजें एक क्षण में तो संसिद्ध नहीं हो सकतीं परन्तु इनके लिए हमें प्रयत्न तो करना ही होगा और जब ये संसिद्ध हो जायें तब फिर प्रयास समाप्त। यदि हम 'उससे' जुड़ गये तो हम 'उसके' लिए स्वतः ही कर्म करेंगे। फिर यह समस्या ही नहीं रहेगी। यही अंतिम रहस्य है। परंतु तीसरे अध्याय में गीता कहती है कि जब तक यह युक्तता की स्थिति नहीं आ जाती तब तक 'मेरे परायण होकर कर्म कर।' श्रीमाताजी की प्रसन्नता के लिए जब हम कर्म करते हों तब हमारा रास्ता खुल जाता है। फिर यांत्रिक प्रकृति में भले ही दूसरे काम चालू रहें परन्तु कामनाओं के दृष्टिकोण से तब हमारे जीवन में कार्य नहीं होते। जब हम उनसे जुड़े हों तो हमें सहज रूप से यह पता लगता है कि वे हमसे क्या चाहती हैं और सहज रूप से हम सब कामों को करते हैं। दूसरे को भले ही वे कर्म कामना के वशीभूत लगें, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसलिए सभी कुछ की यही कुंजी है कि 'मेरे परायण होकर कर्म कर।'
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२।।
६२. इन्द्रियों के विषयों का प्रगाढ़ रुचि से ध्यान करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है; आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है; कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है।
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।।६३।।
६३. क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति विभ्रमित हो जाती है; स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से वह (मनुष्य) नष्ट हो जाता है।
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।।६४।।
६४. परंतु (राग और द्वेष से मुक्त) आत्म-संयमित मनुष्य, आकर्षण-विकर्षण से मुक्त हुई तथा आत्मा के वशीभूत हुई इन्द्रियों के द्वारा विषयों के बीच विचरण करता हुआ परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।।६५।।
६५. उस आत्मप्रसाद (परमानंद) में जीव के सभी दुःखों का अंत हो जाता है; उस आत्मप्रसाद युक्त व्यक्ति में उसकी बुद्धि शीघ्र ही आत्मप्रतिष्ठ हो जाती है।
वह आत्मप्रसाद जीवन के परम सुख का स्रोत है; प्रसादयुक्त जीव को समस्त दुःख स्पर्श करने की सामर्थ्य खोता जाता है; बुद्धि शीघ्र ही आत्मा को शांति में प्रतिष्ठित हो जाती है; दुःख कष्ट नष्ट हो जाता है। इसी आत्मावस्था और आत्मज्ञान में बुद्धि की स्थिर, निष्काम, शोकरहित दृढ़स्थिति को गीता समाधि की संज्ञा देती है।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ।।६६।।
६६. जो मनुष्य (निष्कामयोग से) युक्त नहीं है उसके बुद्धि नहीं होती, चिंतन की एकाग्रता नहीं होती; एकाग्रता-रहित को शांति नहीं मिलती, और अशांत को सुख कैसे हो सकता है?
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ।।६७।।
६७. क्योंकि विषयों के ग्रहण और भोग में विचरती हुई इन्द्रियों के पीछे जो मन अनुसरण करता है वह मन मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार विषयों में खींच कर ले जाता है जिस प्रकार वायु नौका को जल के ऊपर बहा कर ले जाती है।
....इसमें इन्द्रियाँ विषयों से उत्तेजित होकर अशांत, बहुधा भीषण विक्षोभ उत्पन्न करती हैं, उन विषयों को हथियाने और उन्हें भोगने के लिये एक प्रबल अथवा यहाँ तक कि अनियंत्रित अंधाधुंध बहिर्मुखी गति करती हैं और वे अपने साथ इन्द्रिय-मन को वैसे ही खींच ले जाती हैं, 'जैसे समुद्र में वायु नौका को खींच ले जाती है; फिर इन्द्रियों की इस बहिर्मुख गति द्वारा जगाये हुए भावावेगों, आवेशों, लालसाओं और प्रेरणाओं से पराभूत हुआ मन, उसी प्रकार, बुद्धि को खींच ले जाता है जिससे बुद्धि अपना स्थिर विवेक और प्रभुता खो बैठती है।
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।६८।।
६८. इसलिये हे महाबाहो अर्जुन! जिसने इन्द्रियों की सब ओर से उनके विषयों के प्रति उत्तेजना का निग्रह कर दिया है, उसकी बुद्धि (आत्मा में) दृढ़प्रतिष्ठ होती है।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥
६९. जो सभी प्राणियों के लिये रात्रि है उसमें आत्मसंयमी मनुष्य जागता है; जिसमें सभी प्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनि के लिये रात्रि होती है।
वह भी उन्हीं तथ्यों को देखता है जिन्हें हम देखते हैं, किन्तु वह 'कृत्स्नवित्' (समग्र सत्य को जानने वाले) की उच्चतर दृष्टि से देखता है जबकि हम सर्वथा अपने आंशिक ज्ञान, 'अकृत्स्नवित्', की अत्यधिक सीमित मानसिकता से देखते हैं, जो कि एक अज्ञान ही है। हम जिस स्वाधीनता पर गर्व करते हैं वह उसके लिए बंधन है।.... जिसे हम अपनी साधारण मनोवृत्ति के अनुसार स्वाधीन इच्छा कहते हैं, और ऐसा कहने में एक सीमित हद तक औचित्य भी रखते हैं, वह उस योगी की दृष्टि में, जो ऊपर उठ चुका है और जिसके लिए हमारी रात तो दिन है और हमारा दिन रात है, यह कतई स्वाधीन इच्छा नहीं है अपितु प्रकृति के गुणों की अधीनता है।
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।।७०।।
७०. जिस प्रकार सदा भरे जाते रहने पर भी सदा निश्चल, (अपनी मर्यादा में) स्थिर रहने वाले समुद्र में जल प्रवेश करते हैं उसी प्रकार जिसमें समस्त कामनाएँ प्रवेश करती हैं वह शांति को प्राप्त होता है, वह नहीं जो काम्य पदार्थों की कामना करने वाला है।
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।।७१।।
७१. जो मनुष्य समस्त कामनाओं का परित्याग कर के 'मैं' या 'मेरे' की भावना से रहित, स्पृहा-लालसा से रहित होकर कर्म करता है, व्यवहार करता है वह मनुष्य शांति को प्राप्त होता है।
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥
७२. हे पार्थ ! यह ब्राह्मी स्थिति (ब्रह्म में दृढ़ प्रतिष्ठा) है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य और अधिक विमोहित नहीं होता; अपने जीवन के अंतिम समय में भी इस अवस्था में स्थित हो जाने पर मनुष्य ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है।
यह ब्रह्मनिर्वाण बौद्धों का अभावात्मक आत्म-विध्वंस नहीं है, अपितु पृथक् वैयक्तिक आत्मा का उस एक अनंत निर्व्यक्तिक सत्ता के विराट् सत्य में महान् निमज्जन या तल्लीन होना है।
हमारे जीवन के मानदण्ड और मूल्य ही विपरीत हो जाते हैं। जो हमें दिन दिखता है वह आत्मसंयमी मनुष्य के लिए रात्रि होती है और हमें जो रात दिखती है वह उसे दिन दिखाई देता है। रात और दिन का अर्थ यह है कि जहाँ हमें लगता है सब काम बहुत ही अच्छा हो रहा है वह उसके लिए अंधकार हो सकता है और जहाँ हम देखते हैं कि बहुत बुरा हो गया वह उसके लिए बहुत अनुकूल समय हो सकता है। क्योंकि उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है और जिसे हम सफलता कहते हैं वह उसके लिए असफलता है, और जिसे हम असफलता कहते हैं वह उसके लिए सफलता है। परन्तु इस सबसे हमें यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि गीता में वह योग बता दिया गया है जिससे कि यह काम सिद्ध हो सकता है। यह तो केवल एक व्यापक चित्रण किया जा रहा है कि ऐसी-ऐसी चीजें होनी चाहिये। परंतु ये हम कैसे करेंगे वह तो अब शुरू होगा। इस क्रम में पहले निष्काम कर्म बताएँगे। परंतु शुरू में तो निष्काम कर्म हो ही नहीं सकते और न ही यह पता लगता कि कर्तव्य-अकर्त्तव्य क्या है। इसलिए व्यक्ति यज्ञ रूप से कर्म करना आरम्भ करता तो है परन्तु वह यज्ञ पहले तामसिक होता है, फिर राजसिक और फिर सात्त्विक। व्यक्ति श्रीमाताजी की प्रसन्नता के लिए भी यदि कर्म कर रहा हो तब भी शुरू में उनमें मिलावट तो रहती ही है। इस प्रकार यज्ञ का आरोहण चलता है।
इस प्रकार दूसरा अध्याय 'सांख्ययोग' समाप्त होता है।
तीसरा अध्याय
I. कर्म और यज्ञ
बुद्धियोग तथा ब्राह्मी स्थिति में उसकी परिसमाप्ति, जो गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम भाग का विषय है, उसमें गीता की बहुत कुछ शिक्षा बीज-रूप में आ गयी है इसका निष्काम कर्म, समत्व, बाह्य संन्यास का वर्जन और भगवद्भक्ति, ये सभी सिद्धांत इसमें आ गये हैं। परन्तु अभी ये सब बहुत ही अल्प और अस्पष्ट रूप में हैं। जिस बात पर अभी तक सबसे अधिक बल दिया गया है वह है मानव क्रियाओं के सामान्य हेतु, कामना, से इच्छाशक्ति को पीछे खींच लेना तथा आवेशों और अज्ञान के साथ इंद्रियसुख के पीछे दौड़नेवाले विचार और संकल्पमय उसके सामान्य प्राकृत स्वभाव से और अनेक शाखा-प्रशाखाओं से युक्त संतप्त विचारों और इच्छाओं में भटकते रहने के उसके अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि को हटा देना और ब्राह्मी स्थिति की निष्काम स्थिर एकता और निर्विकार प्रशान्ति में पहुँच जाना। इतना अर्जुन ने समझ लिया है। वह इस सब से अपरिचित नहीं है; क्योंकि उस समय की प्रचलित शिक्षा का यही सार था जो मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने के लिये ज्ञान का मार्ग तथा जीवन और कर्म से संन्यास का मार्ग दिखा देता था। बुद्धि का इन्द्रियबोध से, विषय-वासनाओं से तथा मानव-कर्म से हटकर उस परम् में, उस उच्चतम, एकमेवाद्वितीय अकर्त्ता पुरुष में, उस अचल निराकार ब्रह्म की ओर अभिमुख होना ही ज्ञान का सनातन बीज है। यहाँ कर्मों के लिये कोई स्थान नहीं, क्योंकि कर्म अज्ञान से संबद्ध होते हैं; कर्म ज्ञान का ठीक विलोम है; इसका बीज है कामना और उसका फल है बंधन। यही कट्टर दार्शनिक मत है और श्रीकृष्ण भी इसे सर्वथा स्वीकार करते प्रतीत होते हैं, जब वे कहते हैं कि कर्म बुद्धियोग की अपेक्षा अत्यधिक निम्न श्रेणी के होते हैं। और फिर भी योग के अंग के रूप में कर्मों पर बल दिया जाता है; इस तरह इस शिक्षा में एक मूलगत असंगतता प्रतीत होती है। इतना ही नहीं; क्योंकि निःसंदेह (ज्ञान की अवस्था में भी) कुछ काल तक किसी प्रकार का कोई कर्म बना रह सकता है, ऐसा कर्म जो अल्पतम तथा अत्यंत निरापद प्रकार का हो, पर यहाँ जो कर्म बताया जा रहा है वह तो ज्ञान के, सौम्यता के और स्वांतःसुखी जीव की अचल शान्ति के सर्वथा विरुद्ध है, यह तो एक ऐसा कर्म है जो भयानक, यहाँ तक कि राक्षसी कर्म है, रक्तरंजित संघर्ष है, एक निर्मम संग्राम है, एक दैत्याकार सामूहिक नरसंहार है। फिर भी इसी कर्म का यहाँ आदेश किया जा रहा है और फिर इस कर्म के औचित्य का समर्थन किया जा रहा है अंतःस्थ शान्ति और निष्काम समता तथा ब्राह्मी स्थिति की शिक्षा से! यह ऐसा विरोधाभास है जिसका अभी समाधान नहीं हुआ है।
अर्जुन उवाच
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।। १।।
१. अर्जुन ने कहाः हे जनार्दन ! यदि कमाँ की अपेक्षा बुद्धियोग या ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हो तो हे केशव! इस भीषण कर्म में आप मुझे क्यों नियुक्त करते हो।
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्वित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ।। २॥
२. मिले-जुले और जटिल वचन से आप मेरी बुद्धि को मोहित (संभ्रान्त) कर रहे हो; जिससे मैं अपने परम कल्याण को प्राप्त कर सकूँ उस एक ही बात को निश्चित रूप में कहिये।
अर्जुन शिकायत करता है कि उसे परस्पर विरोधी और भ्रमित करने वाली शिक्षा दी गई है, ऐसा कोई स्पष्ट और सुनिश्चित सीधा मार्ग नहीं दिखाया गया जिससे मनुष्य की बुद्धि सीधे प्रभावी रूप से परम कल्याण तक पहुँच जाए। इसी आपत्ति का उत्तर देने में गीता तुरंत ही अपने सुनिश्चित और अलंघनीय कर्म-सिद्धांत का अधिक स्पष्ट प्रतिपादन आरम्भ करती है।
श्रीभगवान् उवाच
लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ।। ३॥
३. श्रीभगवान् ने कहाः हे अनघ (निष्पाप) अर्जुन ! इस लोक में मैंने (ब्राह्मी स्थिति में प्रवेश करने के लिए) द्विविध निष्ठा और साधन मार्ग पूर्व काल में कहे हैं; सांख्यों का ज्ञानयोग के द्वारा और योगियों का कर्मयोग के द्वारा।
श्रीगुरु सर्वप्रथम मोक्ष के उन दो साधनों में भेद करते हैं जिन पर इस लोक में मनुष्य अलग-अलग ध्यान दे सकते हैं, एक है ज्ञानयोग और दूसरा है कर्मयोग। साधारण मान्यता ऐसी है कि ज्ञानयोग कर्मों को मुक्ति का बाधक कहकर त्याग देता है और कर्मयोग इनको मुक्ति का साधन मानकर स्वीकार करता है। वे अभी इन दोनों के संलयन पर, इन दोनों का विभाजन करनेवाले विचार में सामंजस्य स्थापित करने पर बहुत अधिक बल नहीं दे रहे हैं, अपितु यह दर्शाते हुए आरम्भ करते हैं कि सांख्यों का संन्यास, भौतिक (कर्म) संन्यास न तो एकमात्र मोक्ष-मार्ग है और न कर्मयोग से उत्तम ही है। नैष्कर्म्य अर्थात् कर्म-रहित शान्त शून्यता अवश्य ही वह अवस्था है जो पुरुष को प्राप्त करनी है; क्योंकि कर्म प्रकृति के द्वारा होता है और पुरुष को सत्ता की कर्मण्यताओं में लिप्त होने की अवस्था से ऊपर उठकर उस शान्त कर्म-रहित अवस्था और सम-स्थिति में पहुँचना होगा जहाँ से वह प्रकृति के कर्मों का अवलोकन तो कर सके, पर उनसे प्रभावित न हो। यही वास्तव में पुरुष के नैष्कर्म्य का अभिप्राय है, न कि प्रकृति के कर्म का विराम। इसलिए यह सोचना एक भूल है कि किसी प्रकार का कर्म न करने से ही नैष्कर्म्य अवस्था को पाया और भोगा जा सकता है। मात्र कर्मों का संन्यास मुक्ति का पर्याप्त, यहाँ तक कि सर्वथा उचित साधन भी नहीं है।
न कर्मणामनारम्भात्रैष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ।। ४ ।।
४. मनुष्य कमाँ के परिहार से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं करता और केवल (कर्मों का) संन्यास कर देने मात्र से अपनी सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है।
पर यह (कर्मों का संन्यास) अन्य साधनों में से कम-से-कम एक आवश्यक, अनिवार्य और अलंघनीय साधन तो होगा ही? क्योंकि यदि प्रकृति के कर्म जारी रहें तो पुरुष के लिये यह कैसे संभव है कि वह उनमें लिप्त न हो? यह कैसे संभव है कि मैं युद्ध भी करूँ और अपने अन्दर यह न समझै, यह न अनुभव करूँ कि मैं, अमुक व्यक्ति युद्ध कर रहा है, न तो विजय-लाभ की कामना करूँ और न हारने पर अन्दर दुःखी ही होऊँ? यही सांख्यों की शिक्षा है कि जो मनुष्य प्रकृति की क्रियाओं में संलग्न होता है उसकी बुद्धि अहंकार, अज्ञान और कामना में फँस जाती है और इसलिए वह कर्म में प्रवृत्त होती है; इसके विपरीत, बुद्धि यदि निवृत्त हो जाए, पीछे हट जाए, तो इच्छा और अज्ञान की समाप्ति के साथ कर्म का भी अवश्य ही अंत हो जाता है। इसलिए मोक्षमार्ग की ओर गति में संसार और कर्म का परित्याग एक आवश्यक अंग, अपरिहार्य अवस्था और अनिवार्य अंतिम साधन है। उस समय की विचार-पद्धति का यह आक्षेप भगवान् गुरु तुरंत ही पूर्वाभास कर लेते हैं - यद्यपि अर्जुन के मुख से यह बात स्पष्टतः प्रकट नहीं हुई है, परंतु यह उसके मन में है जैसा कि उसकी बाद की बातचीत से झलकता है। वे कहते हैं कि, नहीं, इस प्रकार के संन्यास का अनिवार्य होना तो दूर रहा, ऐसे संन्यास का होना ही संभव नहीं है।
न हि कश्वित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।। ५।।
५. क्योंकि कोई भी पुरुष कभी क्षणभर के लिये भी बिना कर्म किये नहीं रहता; प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश हुआ कर्म करने में प्रवृत्त किया जाता है।
इस महान् विश्वकर्म का और विश्वप्रकृति की शाश्वत् क्रियाशीलता और शक्ति का यह स्पष्ट और प्रबल अनुभव, जिस पर तांत्रिक शाक्तों ने आगे चलकर बहुत बल दिया और यहाँ तक कि प्रकृति या शक्ति को पुरुष से भी श्रेष्ठ बना दिया, गीता की एक बड़ी ही विलक्षण विशेषता है। यद्यपि यहाँ इसका मृदु संकेतमात्र है, फिर भी, इसके विचार के उन तत्त्वों की शिक्षा के साथ, जिन्हें हम ईश्वरवादी और भक्तिवादी तत्त्व कह सकते हैं, मिलकर यह महिमा इतनी पर्याप्त सशक्त हो गयी कि योगमार्ग में कर्म की सक्रियता या गतिशीलता को लागू कर के प्राचीन दार्शनिक वेदांत की निवृत्तिपरक वृत्ति का इसमें इतने प्रभावी रूप से रूप-परिवर्तन कर दिया गया है। प्राकृतिक जगत् में देहधारी मनुष्य एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता; यहाँ (पृथ्वी पर) उसका अस्तित्वमात्र ही एक कर्म है, संपूर्ण ब्रह्माण्ड ईश्वर का एक कर्म है, केवल जीना भी उसी की एक गति या क्रिया है।
हमारा दैहिक जीवन, उसका पालन, उसकी निरंतरता एक यात्रा है, एक शरीरयात्रा है, और कर्म के बिना वह पूरी नहीं हो सकती। परन्तु यदि कदाचित् कोई मनुष्य अपने शरीर को देख-रेख से वंचित भी रख सकता हो, यों ही बेकार छोड़ सकता हो, किसी वृक्ष की तरह सदा स्थिर खड़ा रह सकता हो या पत्थर-सा अचल बैठा रह सकता हो, 'तिष्ठति' तो भी इस स्थावर या स्थूल अचलता द्वारा भी वह प्रकृति के हाथ से नहीं बच सकता; प्रकृति को क्रियाओं से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि कर्म का अभिप्राय केवल हमारी शारीरिक गतियों (चलना-फिरना आदि) और अन्य क्रियाओं से हो नहीं है, हमारा मानसिक जीवन भी तो एक बहुत बड़ा जटिल कर्म है, अपितु चंचला प्रकृति के कर्मों का यही अधिक विशाल और अधिक महत्त्वपूर्ण अंग है - हमारे बाह्य दैहिक (कर्म) का यही आंतरिक कारण और नियामक है। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला यदि हम फलस्वरूप होनेवाले बाह्य प्रभाव का तो निग्रह करें पर उसके आंतरिक कारण की क्रिया को जारी रखें। इन्द्रियों के विषय हमारे बंधन के केवल सहायक कारण हैं, मन का उन विषयों पर आग्रह ही इस बंधन का माध्यम और मूल कारण है।
अर्जुन भगवान् को कहता है कि एक ओर तो वे उसे शांत बने रहने का उपदेश कर रहे हैं और दूसरी ओर उसे घोर कर्म में लगा रहे हैं। वह शिकायत करता है कि ये सब तो मिश्रित बातें हैं। एक ओर वे कछुए का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि इन्द्रियों को बाहर जाने से रोकना होगा, उन पर अंकुश लगाना होगा और दूसरी ओर युद्ध की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का घोर कर्म शांत भाव से कैसे संभव है? इसलिए अर्जुन कहता है कि 'आपकी बातें तो बुद्धि को भ्रमित करने वाली हैं। यदि आप मानते हैं कि बुद्धियोग श्रेष्ठ है तो इस प्रकार के घोर कर्म में लगाने की अपेक्षा मुझे उसी की शिक्षा दीजिये। मेरे लिए जो उपयोगी हो वही एक निश्चित बात बताइये।' तब भगवान् कहते हैं कि आरंभ से ही 'मैंने दो रास्ते बताए हैं। सांख्य-योगियों का ज्ञानमार्ग और कर्मयोगियों का कर्ममार्ग।' परंतु दोनों का ही तत्त्वतः निरूपण करने के बाद भगवान् कहते हैं कि ये दोनों ही मार्ग केवल दिखने में ही भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु जो वास्तव में जानता और समझता है उसके लिए ये एक ही हैं। सांख्य योग कहता है कि सभी कर्मों का त्याग कर दो। परंतु कर्म किये बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, चूंकि कर्म केवल शरीर के द्वारा ही नहीं होते अपितु बुद्धि से की जाने वाली क्रियाएँ, प्राण की सारी भावनाएँ, आवेग आदि, और यहाँ तक कि श्वास-प्रश्वास भी कर्म में ही समाहित होते हैं। पत्थर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्म करता है। क्योंकि जहाँ भी वह होगा वहाँ हवा और जल के बहाव में बाधा उत्पन्न करेगा। प्रश्न इतना ही है कि कर्म की प्रतिष्ठा अहं में है या फिर वे परमात्मा के नियत किये जाते हैं। इसलिए गीता आगे चलकर सांख्य और कर्म में समन्वय साधेगी कि किस प्रकार ये दोनों केवल दिखने में ही भिन्न-भिन्न हैं पर वास्तव में एक ही हैं। बुद्धि योग में व्यक्ति बुद्धि के द्वारा कर्मों का नियोजन करता है और निष्काम कर्म में व्यक्ति को बुद्धि की सहायता लेनी होगी, अपने समर्पण की सहायता लेनी होगी। वास्तव में तो व्यक्ति को अपने कर्मों को परमात्मा के निमित्त करना आरंभ करना होगा।
परंतु जब बात यह आती है कि 'मेरी प्रसन्नता के निमित्त कर्म करो' तो अर्जुन पूछता है क्या आप इससे प्रसन्न होंगे कि 'मैं इन सबको मार डालूँ? क्या यह कोई अच्छा काम होगा?' ऐसा प्रश्न स्वभावतः ही उठ खड़ा होता है जिसके उत्तर में भगवान् अपने-आप का काल-पुरुष के रूप में प्राकट्य करते हैं और कहते हैं कि 'मैं इनका विनाश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और तेरे चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा, तू तो इसका बस निमित्त बन, 'निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्' क्योंकि इन सबका अन्त होना तो निश्चित है। इसलिए चूँकि यह मेरे द्वारा निर्धारित की गई नियति है इसलिए इसके लिए काम करने में ही मेरी प्रसन्नता है।' अतः चूंकि भगवान् वह कर्म करवाना चाहते हैं इसलिए वही करने योग्य कर्म है। क्योंकि बुद्धि योग से या अन्य किसी भी योग के माध्यम से तो इस प्रकार के घोर कर्म की शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। यदि व्यक्ति परमात्मा के लिए जीना चाहता है तो परमात्मा की जो इच्छा होगी वही कर्म वह करना चाहेगा। परन्तु इस सारी चीज को गीता शनैः-शनैः विकसित करेगी।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।। ६।।
६. जो मनुष्य अपनी कर्मेन्द्रियों का संयम करता है परंतु मन से विषयों का स्मरण करता और उनमें रमण करता रहता है वह मूढ़बुद्धि है और उसकी आत्मसंयम की प्रणाली को मिथ्याचार कहा जाता है।
संभव है कि कोई व्यक्ति कर्मेन्द्रियों का नियंत्रण कर उन्हें उनकी स्वाभाविक क्रीड़ा करने से रोक दे, परंतु इससे उसका कोई लाभ नहीं यदि उसका मन इन्द्रियों के विषयों का ही स्मरण और चिंतन करना जारी रखे। ऐसे मनुष्य ने तो आत्म-संयम की मिथ्या धारणाओं से स्वयं को भरमाया हुआ ही है; उसने न तो संयम के उद्देश्य को न उसके मर्म को समझा है, न अपने अंतःकरण के मूल तत्त्वों को ही समझा है; इसलिए संयम के उसके सभी तरीके मिथ्या और व्यर्थ हैं, मिथ्याचार' हैं। शरीर के कर्म, और मन से होनेवाले कर्म भी अपने-आप में कुछ नहीं हैं, न वे बंधन हैं न बंधन के मूल कारण ही। मुख्य बात है प्रकृति की वह प्रबल शक्ति जो मन, प्राण और शरीर के अपने महान् क्षेत्र में अपनी मनमर्जी व अपनी क्रीड़ा करेगी, उसमें खतरनाक चीज है उसके त्रिगुण की वह शक्ति जो बुद्धि को मोहित और भ्रमित कर देती है और इस तरह आत्मा को आच्छादित कर देती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कर्म और मोक्ष के संबंध में गीता का सारा मर्म या महत्त्वपूर्ण बिन्दु यही है। त्रिगुण के व्यामोह और व्याकुलता से मुक्त हो जाओ, फिर कर्म जारी रह सकता है, क्योंकि वह तो होता ही रहेगा; फिर वह कर्म चाहे जितना भी विशाल हो, समृद्ध हो या कैसा भी विकट और भीषण हो, उसका कुछ महत्त्व नहीं, क्योंकि तब पुरुष को उसकी कोई चीज छू नहीं सकती, जीव नैष्कर्म्य की अवस्था को लाभ कर चुका होता है।
परन्तु इस बृहत्तर बिन्दु तक गीता अभी नहीं पहुँची है। चूंकि मन ही मूल कारण है, चूंकि अकर्म असंभव है, तब यही युक्ति-संगत, आवश्यक और उचित है कि आंतर और बाह्य कर्मों को संयमित रूप से किया जाए।
यहाँ यह समस्या बड़ी विकट है। अवश्य ही गीता में तो इस समस्या के बारे में विस्तार से वर्णन नहीं है क्योंकि ऐसा किये जाने की इससे आशा नहीं की जा सकती। त्रिगुण क्या हैं? उनकी कार्य प्रणाली क्या है? किस प्रकार से हम जो भी कर्म करते हैं उनमें ये व्याप्त रहते हैं? पहला विषय तो यह है कि ये हमारी कर्मेन्द्रियों को वश में रखते हैं, और हम अपने विषयों में विचरण करने से अपने को रोक नहीं पाते। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो गीता कहती है कि वह मिथ्याचारी है। यदि वह सारे समय रहता तो विषयों के चिंतन में है परंतु बाहर अभिव्यक्त होने से उन्हें रोकता है तो वह एक बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति में होगा और इससे तो उसकी अपनी सत्ता में ही अन्तर्विरोध उत्पन्न हो जाएगा। चौबीसों घण्टे उसे इस अन्तर्विरोध का सामना करना होगा। और ऐसे निग्रह से वह अपनी सारी ऊर्जाओं को क्षय कर देगा, नष्ट कर देगा।
परंतु इससे श्रेष्ठतर है संयम। व्यक्ति न केवल कामनामय कर्मों को ही नहीं करता अपितु उससे संबंधित किसी प्रकार के विचार को भी अपने मन में प्रवेश नहीं करने देता। तब फिर सत्ता में कोई अन्तर्विरोध नहीं रहता। जब एक बार व्यक्ति को गहराई से समझ में आ जाए कि किसी काम को नहीं करना है, तो उसे अपने मन को भी उससे मुक्त रखने की सामर्थ्य होनी चाहिये, क्योंकि यदि ऐसा न किया जाए तो यह स्वयं का ही निषेध होगा। जब भी कोई गलत ऊर्जा या स्पंदन से आती चीज पता लग जाए तो अपना द्वार बंद कर लो और कहो कि 'भाड़ में जाओ मैं यह न तो करने वाला हूँ न इसके बारे में सोचने ही वाला हूँ।' श्रीमाँ ने यही समाधान बताया है।
----------------
'मैं नहीं सोच सकता कि मिथ्याचारी का अर्थ पाखण्डी हो सकता है। वह व्यक्ति पाखण्डी कैसे होगा जो अपने-आप पर इतना भारी कष्ट या अभाव लाद देता है? वह भूल में है और भ्रम में है, 'विमूढ़ात्मा' है और उसका आचार, अर्थात् आत्म-संयम का लोकाचार द्वारा नियमन का तरीका, मिथ्या और व्यर्थ है- अवश्य ही गीता का यहाँ यही अभिप्राय है।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।। ७।।
७. हे अर्जुन! जो मनुष्य मन के द्वारा इन्द्रियों को संयत कर के अनासक्त होकर कर्मेन्द्रियों के द्वारा कर्मयोग का अनुष्ठान करता है वह श्रेष्ठ है।
बुद्धि के यंत्र के रूप में मन को चाहिए कि वह इन्द्रियों को अपने वश में करे और तत्पश्चात् कर्मेन्द्रियों को उनके उचित कर्म के अनुसार प्रयोग में ले, ऐसे कर्म में प्रयोग करे जो योगस्वरूप किया जाता है। पर इस आत्मसंयम का सच्चा आशय क्या है, कर्मयोग का अभिप्राय क्या है? कर्मयोग का अभिप्राय है अनासक्ति; मन से इन्द्रियों के विषयों से और कर्मों के फल से अलिप्त रहते हुए कर्म करना। संपूर्ण अकर्म नहीं, संपूर्ण अकर्म तो भूल है, भ्रम है, आत्म-वंचना है और असंभव है, किन्तु वह कर्म जो पूर्ण और स्वतंत्र हो, इन्द्रियों और आवेशों के वश होकर न किया गया हो ऐसा निष्काम और आसक्ति रहित कर्म ही सिद्धि का प्रथम रहस्य है।
इन तीनों गुणों को हम आसानी से संभाल नहीं सकते। इसके लिए यह आवश्यक है कि इनसे ऊपर उठा जाए जो कि आसान नहीं है। परंतु फिर भी हमें यह शुरू तो करना ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि हम शुरू कैसे करें? उसके लिए कह रहे हैं कि व्यक्ति के कर्म उसके सही-गलत, उचित-अनुचित के बोध के द्वारा संचालित होने चाहिए, भले वह बोध वर्तमान में कितना भी सीमित क्यों न हो। यह पहली चीज है। व्यक्ति के जो भी मापदंड हों, भले ही वे कितने भी ऊँचे या नीचे हों, पर उन्हीं के द्वारा उसे अपने कर्मों का संचालन करना सीखना होगा। जैसे-जैसे उसकी समझ बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे वह महत्तर कर्म करता जायेगा। परंतु जब तक व्यक्ति के कर्म कामना या लालच आदि के द्वारा या फिर भौतिक आवेगों के द्वारा या फिर मन के छिछले विचारों के द्वारा चालित होंगे तब तक इनसे कोई मुक्ति संभव नहीं है। परंतु यहाँ श्रीकृष्ण माँग करते हैं कि अपनी बुद्धि को अपनी सत्ता की गहराई में किसी चीज से युक्त कर दो, "युक्त आसीत मत्परः" और उस बुद्धि को अपने कर्मों का निर्देशन करने दो। इस बुद्धि के अनुसार हम जिस चीज को अनुचित मानते हैं, गलत मानते हैं उसे करने से हमें पूर्णतया निषेध करना होगा और ऐसा करने में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी सत्ताएँ और शक्तियाँ हैं जो हम पर नियंत्रण कर लेती हैं और हमें इंद्रियों के पीछे, कामनाओं और आवेगों के पीछे जाने को बाध्य कर देती हैं और उन सत्ताओं को 'ना' सुनने की आदत नहीं है। फिर भी जो बुद्धि परमात्मा से युक्त है वह इन सब पर नियंत्रण कर पायेगी क्योंकि जितना ही व्यक्ति भगवद्-परायण होगा उतनी ही सहायता उसे सब निम्न शक्तियों पर नियंत्रण हेतु प्राप्त होती रहेगी। अतः प्रथमतः हमें उन पर युक्त बुद्धि द्वारा नियंत्रण करना सीखना होगा। ऐसा करना ही होगा। तब फिर अर्जुन पूछता है कि मैं ऐसा कैसे करूँ? इसके उत्तरस्वरूप भगवान् कहते हैं 'मा फलेषु कदाचन', कि फल में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर्म इसलिये नहीं करना है कि उससे कुछ प्राप्त हो जाए। अपितु वह इसलिये करना है क्योंकि वह करना उचित है। अब व्यक्ति यह कैसे पता करे कि सही और गलत क्या है? इसी के उत्तर में भगवान् आने वाले श्लोक में कहते हैं कि 'नियत कर्म कर।'
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ।। ८।।
८. तू नियत कर्म कर; क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ होता है और कर्म बिना किये तेरे शारीरिक जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता।
----------------
* मैं नियतं कर्म के इन दिनों लगाए जाने वाले अर्थ को स्वीकार नहीं कर सकता जो उसकी व्याख्या इस रूप में करता है मानो इसका अर्थ उन नियत-निर्धारित तथा कर्मकाण्डपरक औपचारिक कर्मों से हो और जो कर्म वैदिक नित्यकर्म के समरूप ही हो अर्थात् नियमित यज्ञ-अनुष्ठानादि कर्म तथा वैदिक जीवन के नित्य के विधि-विधान। निश्चय ही पिछले श्लोक के 'नियम्य' शब्द का तात्पर्य लेकर ही इस लोक में 'नियत' शब्द प्रयुक्त हुआ है।... किसी बाह्य विधान या नियम द्वारा निर्धारित औपचारिक कर्म नहीं, अपितु मुक्त बुद्धि द्वारा नियत किया हुआ निष्काम कर्म ही गीता की शिक्षा है।
इस प्रकार भगवान् कहते हैं कि नियत कर्म करो, 'नियतं कुरु कर्म त्वं, मैंने यह कहा है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान, बुद्धि श्रेष्ठ है... पर मेरा आशय यह नहीं था कि कर्म से अकर्म श्रेष्ठ है, सत्य इसके विपरीत है अर्थात् अकर्म की अपेक्षा कर्म ही श्रेष्ठ है, 'कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। कारण, ज्ञान का अर्थ कर्म का संन्यास नहीं है, इसका अर्थ है समता, तथा कामना और इन्द्रियों के विषयों से अनासक्ति; और इसका अर्थ है बुद्धि का उस आत्मा में स्थिर-प्रतिष्ठ होना जो स्वतंत्र है, प्रकृति के निम्न साधनों अथवा उपकरणों के बहुत ऊपर है और वहीं से मन, इन्द्रियों और शरीर के कर्मों को आत्मज्ञान की तथा आध्यात्मिक अनुभूति के विशुद्ध निर्विष्य आत्मानंद की शक्ति द्वारा नियत करता है।...बुद्धियोग कर्मयोग द्वारा परिपूर्ण होता है; आत्म-मुक्ति को देनेवाला बुद्धियोग निष्काम कर्मयोग द्वारा अपनी पूर्ण सार्थकता प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता अपनी निष्काम कर्म की आवश्यकता के सिद्धांत को स्थापित करती है, और सांख्यों की (आत्मनिष्ठ) ज्ञान-साधना को - मात्र उनकी बाह्य विधि का परित्याग कर के योग की साधना के साथ एक करती है।
परन्तु फिर भी एक मूल समस्या अभी तक बिना समाधान के बची रहती है। कठिनाई यह है कि हमारा वर्तमान स्वभाव जैसा है उसके रहते, और उसके कर्म के सामान्य प्रेरक तत्त्व के रूप में कामना के रहते हुए एक यथार्थतः निष्काम कर्म करना कैसे संभव है?... एकमात्र यज्ञ को लक्षित कर के सभी कर्मों का निर्वहन करने से, यही है श्रीगुरु का उत्तर।
यह बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तो, हम किसी कर्म का क्रियान्वयन कैसे करते हैं? सामान्यतया हमें कुछ चीजें प्राप्त करने की इच्छा होती है और कुछ चीजें नहीं चाहिये होती हैं, और इसी के अनुसार हम अपने कर्मों का निर्धारण करते हैं। जब तक हम इस प्रकार कर्म करते हैं तब तक हम प्रकृति के दुश्चक्र में फंसे रहते हैं और कभी भी इससे ऊपर नहीं उठ सकते। तब फिर इसके लिए क्या किया जाए? पहली चीज तो है कि कामना के वशीभूत होकर कर्म न करना। तथा इस दृष्टिकोण से भी नहीं करना कि उस कर्म का हमारे लिये क्या परिणाम होगा। सबसे पहले तो हमें कर्म के फल के विषय में उदासीन होना होगा। हमें यह देखना होगा कि सही या उचित कर्म क्या है और उसी अनुसार कर्म करना होगा, भले उससे तथाकथित सुख आता है या दुःख, व्यक्ति को उससे उदासीन रहता होता है। तभी नियत कर्म किये जा सकते हैं। अब इसका पता कैसे लगाएँ कि सही कर्म कौन सा है? क्योंकि जब हमारी बुद्धि आच्छादित है, हमारा हृदय कामनाओं और आवेगों से प्रताड़ित है और शरीर भी तम से आच्छादित है, ऐसे में जब तक हमारी बुद्धि भगवान् से जुड़ी हुई नहीं है, तब तक वह हमें सही सूचना नहीं दे सकती। वास्तव में अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा नहीं कहता परंतु उसके मन में तो यह अवश्य है ही कि यदि फल के अनुसार कर्म करना हो तो व्यक्ति निर्धारित कर सकता है कि अमुक कर्म उसे करना है और अमुक कर्म से बचना है। व्यक्ति को कोई चीज की इच्छा है तो वह अमुक कर्म कर सकता है अन्यथा नहीं, परंतु यदि कोई फल की आशा नहीं रखनी है, तब फिर वह निर्णय कैसे करे कि क्या करना चाहिये और किससे बचना चाहिये। अब इसका एक तर्कसंगत उत्तर आता है कि 'यज्ञ के रूप में कर्म करो'। अर्थात् 'मेरी प्रसन्नता के निमित्त कर्म करो'। और यह तो व्यक्ति को ही कल्पना करनी होगी कि भगवान् क्या पसन्द करते हैं और क्या नापसंद करते हैं। हाँ, शुरू में तो यह कल्पना एकदम सही तो नहीं होगी, परंतु फिर भी यह एक अच्छी शुरुआत होगी। भगवान् कहते हैं कि कमर्मों का तुम्हारा सिद्धांत होना चाहिये कि 'मुझे क्या पसंद आएगा और क्या पसंद नहीं आएगा।' और यह तो एक बड़ा भारी काम है। इसमें व्यक्ति अधिकाधिक यह पाता है कि उसके विचारों आदि में भारी मिश्रण है। और मिलावट तब तक रहती है जब तक कि वह अपनी गहनतम गहराइयों तक नहीं पहुँच जाता।
श्रीअरविन्द के अतिरिक्त गीता में यज्ञ के सिद्धांत के निरूपण का क्या औचित्य है इस बात का स्पष्टीकरण कोई नहीं करता। उन्होंने इस यज्ञ के सिद्धांत को एक व्यापक स्वरूप प्रदान कर दिया है, किसी देश-काल तक ही सीमित नहीं रखा है। यज्ञ वास्तव में एक परस्पर आदान-प्रदान है। व्यक्ति प्रकृति से कुछ प्राप्त करता है और स्वयं कुछ प्रतिदान करता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है, ब्रह्माण्ड का मूल सिद्धान्त है। यहाँ तक कि जड़तत्त्व भी ऊर्जा का आदान-प्रदान करता है। परमाणु स्तर पर भी सदा ही ऊर्जा का आदान-प्रदान चलता रहता है। इस सिद्धान्त के प्रकाश में श्रीअरविन्द बता रहे हैं कि व्यक्ति कर्म कैसे करे? जब व्यक्ति प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तब उसे पता लगता जाता है कि जिस भाव से वह कर्म करता है वह भी अंतिम या निर्णायक नहीं है। और इसलिए यज्ञ का भी आरोहण होता है। भगवान् को, श्रीमाँ को क्या पसंद है, इस विषय में उसकी समझ भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अध्याय तीन और चार में यज्ञ के सिद्धांत को व्यापक स्वरूप प्रदान करके उसकी व्याख्या की गई है। हमारे सभी कर्म किसी बहुत ही उच्च और गहरी सत्ता को समर्पित होने चाहिए न कि स्वार्थपरता और मात्र शरीर के भरण-पोषण के लिए। निःसंदेह शरीर का भरण-पोषण तो स्वतः हो ही जाएगा, परन्तु केवल शरीर एवं जीवन की रक्षा के लिए ही नहीं अपितु इससे कहीं अधिक हमारी सत्ता के सत्य के लिए, और इसलिए कि पूरे ब्रह्माण्ड के साथ हमारा एकत्व इसकी माँग करता है, अतः वह कर्म भी हम करते हैं क्योंकि हम ब्रह्माण्ड से भिन्न नहीं हैं। सपूर्ण ब्रह्माण्ड में यदि शक्तियों का आदान-प्रदान नहीं होता तो हम जीवित ही नहीं रह सकते थे। इस बात को समझना होगा और इसे उत्तरोत्तर ऊपर के स्तरों तक उठाते जाना होगा। यह यज्ञ का सिद्धांत है।
प्रश्न : शुरुआत में चूँकि हमें इस बात का भान नहीं होता कि कौनसी चीज माँ को प्रसन्न करेगी या उन्हें पसंद आएगी, तो हमें आरंभ तो हमारी इस बुद्धि या समझ से ही करना होगा कि अमुक चीज माँ को प्रसन्न करेगी?
उत्तर : बिल्कुल ! परंतु भले ही व्यक्ति कितना भी स्थूल चेतना में ही क्यों न हो, फिर भी किन्हीं चीजों को तो वह भी इस बहाने से उचित नहीं ठहरा सकेगा कि वे काम श्रीमाँ को प्रसन्न करेंगे। ऐसा करना मुश्किल होगा। हालाँकि शुरू में तो ऐसे काम भी धोखे से घुस आएँगे, परंतु ज्यों-ज्यों यज्ञ का आरोहण होता जाएगा त्यों-त्यों अधिक प्रकाश आता जाएगा और ऐसे कामों पर अधिकाधिक अंकुश लगता जाएगा।
प्रश्न : क्या ऐसा नहीं है कि प्रारम्भिक अवस्था में तो सही-गलत के जो मापदंड हमें सिखाए गए हैं उन्हीं के द्वारा मान कर चलना होगा कि जो चीज मुझे सही लगती है वह श्रीमाँ को पसंद आएगी और जो चीज मुझे सही नहीं लगती वह माँ को भी प्रसन्न नहीं करेगी?
उत्तर : हाँ, ऐसा हो सकता है। परंतु फिर भी समस्या यह है कि इसे हमें अपनी सत्ता पर आरोपित करना होगा। ऐसे समय होते हैं जब हम जानते हैं कि अमुक चीज सही नहीं है परंतु हम उसे करने को बाध्य होते हैं, और कभी-कभी हमें पता होता है कि अमुक काम करने के लिए अच्छा है परंतु उसे करने के लिए आवश्यक शक्ति-सामर्थ्य नहीं होता। वह तो प्रकृति की अपनी शक्ति है और इसका सामना हम कैसे करेंगे? जब तक हम यज्ञ नहीं करते, जब तक आत्म-उत्सर्ग नहीं करते, जब तक हम अपनी गहराइयों और ऊँचाइयों से शक्ति तथा ऊर्जा नहीं प्राप्त करते, तब तक हम अपनी कामनाओं आदि पर प्रभुत्व नहीं प्राप्त कर सकते। इन सहज भावों पर प्रभुत्व नहीं कर सकते कि 'मुझे इस काम से क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या लाभ होने वाला है', और ये ही चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती रहेंगी। परंतु इसी स्थिति से हमें आरंभ करना होता है। परंतु यदि सच्चा आत्मोत्सर्ग हो तो ऐसी शक्तियाँ इस प्रक्रिया के अंदर प्रवेश करती जाएँगी जो हमें अधिकाधिक ऊपर उठाती जाएँगी। यज्ञ के आरोहण में हम ऐसा भली-भाँति देख सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ स्थित है। जब व्यक्ति सबसे नीचे के स्तर पर हो तब वह लोगों से, घटनाओं तथा परिस्थितियों से अधिकतम प्राप्त करना चाहता है और स्वयं न्यूनतम देना चाहता है। उसे जड़त्व का या फिर तमस् का स्तर कहते हैं, जो कि निम्नतम स्तर है। उसके बाद व्यक्ति कुछ अधिक समझदार हो जाता है। वह कहता है कि यदि दूसरों के लिये वह दस काम करेगा तो वे भी बदले में उसके लिए दस काम करेंगे। यदि वह समाज का लाभ करेगा तो समाज भी उसके प्रति अच्छा और उपकारी होगा। इसलिये व्यक्ति इस सोच के साथ काम करता है कि जैसे काम वह करेगा वैसे ही प्रतिफल उसे प्राप्त होंगे। यह राजसिक यज्ञ की अवस्था है। इससे आगे की अवस्था में व्यक्ति बिना किसी प्रत्याशा के, कि कोई उसकी सहायता करता है या नहीं, लाभ मिलता है या नहीं, वह तो केवल सही तरीके से सही चीज ही करना चाहता है, भले उसका परिणाम जो भी क्यों न हो। व्यक्ति वही करता है जो उसकी आत्मा में, उसके हृदय की गहराई में और चेतना के शिखर पर उसे महसूस होता है कि वही करने योग्य कार्य है। तब व्यक्ति सात्त्विक होता है। ये तीनों ही गुण पराश्रित हैं। सत्त्व आश्रित है व्यक्ति की मनस् शक्ति पर, रजस् आश्रित है प्राण-शक्ति पर और तमस् आश्रित है भौतिक शक्ति पर। जब व्यक्ति अंतिम अवस्था, अर्थात् सत्त्व, से भी मुक्त हो जाता है, और सहज रूप से जगदम्बा की शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगती है, तब इसमें फिर सही-गलत, उचित-अनुचित की बातें नहीं रह जातीं, व्यक्ति इतना पारदर्शी बन जाता है कि वह शक्ति उसके द्वारा प्रवाहित होने लगती है और दूसरों तक भी प्रवाहित होने लगती है और सभी कुछ को भगवान् को अर्पित कर देती है। वही यज्ञ की चरम अवस्था है। तब व्यक्ति का जीवन धन्य है। तब व्यक्ति निखैगुण्य हो जाता है, त्रिगुणों से ऊपर उठ जाता है। इस तरह हम सम्पूर्ण जीवन को यज्ञ के आरोहण के रूप में देख सकते हैं।
प्रश्न : जब हम श्रीमाँ की प्रसन्नता के लिए कर्म करना प्रारम्भ करते हैं तो क्या यह निखैगुण्य की ओर बढ़ना है?
उत्तर : अवश्य ही। सम्पूर्ण ऋग्वेद मूलरूप में यज्ञ के आरोहण की साधना है। हमारे सभी कर्मों, विचारों, भावनाओं, सभी ऊर्जाओं, उनकी परस्पर क्रियाओं को इसमें बताया गया है। साथ ही यह बताया गया है कि किस प्रकार उनका सही व्यवस्थापन करना है, कैसे वे भगवान् के साथ जुड़ जाते हैं, और इस सब को विभिन्न देवताओं के प्रतीक के रूप में यज्ञ के रूप में, और भी बहुत से प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से वेद में बताया गया है। सारा वेद यज्ञ के आरोहण को दिखाता है, कि हम सही कर्म कैसे करें, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता है ही नहीं। जब तक हम परम प्रज्ञा से जुड़े हुए नहीं हैं, और उसे ही अपनी सत्ता में कार्य करने का मौका नहीं प्रदान करते, तब तक हम समुचित कर्म नहीं कर रहे होते।
प्रश्न : क्या यज्ञ के आरोहण के साथ-साथ ही आनंद का भी आरोहण होता है?
उत्तर : हाँ, यह तो एक पूर्ण गति है जिसमें ज्ञान, चेतना और आनंद तीनों ही साथ-साथ चलते हैं। इस यात्रा का व्यक्ति इनमें से किसी भी एक के दृष्टिकोण से वर्णन कर सकता है।
प्रश्न : यदि व्यक्ति आनन्द महसूस नहीं कर रहा हो तो क्या तब भी वह उस ओर बढ़ रहा हो सकता है?
उत्तर : यह असम्भव है। यज्ञ एक बहुत ही आनन्ददायक विषय है। यह एक अतिशय आनन्द है। यदि व्यक्ति ऐसा महसूस नहीं करता तो संभवतः वह केवल यज्ञ करने का प्रयास कर रहा है, पर यज्ञ नहीं कर रहा। यह उस अर्थ में यज्ञ नहीं है जैसा कि किसी ने श्रीअरविन्द से पूछा कि प्रभु, ज्ञान के समर्पण का अर्थ क्या है। तो श्रीअरविन्द ने उत्तर दिया कि निश्चय ही इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति ज्ञान को त्याग कर कष्टकर और दृढ़ रूप से भगवान् के लिए अपने को बेवकूफ बना ले। वह तो कदाचित् ही कोई यज्ञ होगा। ज्ञान के यज्ञ का अर्थ है कि ज्ञान को भगवान् की सेवा में नियुक्त कर देना। बजाय इस क्षुद्र व्यक्तित्व की, क्षुद्र अहं की या फिर अपने परिवार, देश, समाज आदि बृहत्तर अहं की सेवा करने के, अपनी बुद्धि दिव्य जननी की सेवा में लगा देना। कर्म के समर्पण का आशय यह नहीं है कि व्यक्ति कोई कर्म न करे। अपितु इसका अर्थ है कि सारे कर्मों का लक्ष्य दिव्य जननी ही होना चाहिए। तब यह पूर्ण होता है। और इसके साथ-ही-साथ ज्ञान, प्रेम, शक्ति, कर्म, आनन्द सभी का एक साथ आरोहण होता है। और एक क्षुद्र संकीर्ण मनुष्यत्व से छूटकर व्यक्ति ऊपर उठ कर दिव्य स्तर तक पहुँच जाता है। गुह्यवादी इसी साधना की दीक्षा देते थे।
हम एक छोटे से क्षुद्र शरीर में कैद हैं जो कि मानो एक बहुत छोटा-सा संकीर्ण पिंजरा है, या फिर अपनी प्राणिक प्रकृति में या फिर एक भिन्न व्यक्तित्व के बोध में कैद हैं, या अधिक से अधिक इस भाव में सीमित हो सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा ही स्वरूप है, परंतु एक विशालतर चेतना में यह सब तो बहुत ही क्षुद्र है। यहाँ तक कि पूरा ब्रह्माण्ड भी उस चेतना के लिए बहुत ही क्षुद्र है। इस ब्रह्माण्ड के परे भी असंख्य अनंतताएँ हैं। परंतु फिर भी हम एक संकीर्ण चेतना में ही सीमित और बद्ध रहते हैं। अधिकांशतः तो हम अपने शरीर से ही बँधे रहते हैं या फिर शरीर से संबंधित रिश्तेदारों से या किसी संकीर्ण धर्म, समाज, देश या मनुष्यजाति से संबद्ध रहते हैं। ये सभी तो बहुत ही क्षुद्र हैं। हम अपने सच्चे स्वरूप में इनसे अनन्त रूप से महत्तर हैं। सभी जगह यही गुह्यवादियों की शिक्षा रही है। गीता व्यवस्थित ढंग से इस की व्याख्या करेगी कि यदि नियत कर्म करना है तो कैसे किया जाए। विचार, भाव, कर्म को महज इस सीमित व्यक्तित्व की सेवा में नियुक्त करने की बजाय कैसे इन्हें पूर्ण रूप से अर्पित किया जा सकता है।
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ।। ९।।
९. यज्ञ के लिये किये जानेवाले कर्म से अन्यथा जो कर्म किये जाते हैं उनसे मनुष्यों का यह लोक (मनुष्य) कर्मों से बद्ध होता है; हे कुंतीपुत्र अर्जुन! अनासक्त होकर यज्ञ के लिये (यज्ञ की भावना से) कर्म कर।
यह स्पष्ट है कि न केवल यज्ञ-कर्म और सामाजिक कर्तव्य ही, अपितु सभी कर्म इसी भाव से किये जा सकते हैं; कोई भी कर्म संकीर्ण या अभिवर्धित अहंभाव से या फिर भगवान् के लिए किया जा सकता है। प्रकृति की सारी सत्ता और सारे कर्म का अस्तित्व केवल भगवान् के लिए ही है; भगवान् से ही उसका उद्भव होता है, भगवान् से ही उसकी स्थिति है और भगवान् की और ही उसकी गति है। परंतु जब तक हम अहंभाव से शासित हैं तब तक हम इस सत्य का बोध प्राप्त नहीं कर सकते, न इस सत्य के भाव में कर्म कर सकते हैं, अपितु हम अहं की तुष्टि के लिए और अहंभाव से, यज्ञ के विपरीत हेतु से कर्म करते हैं। अहंकार बंधन की गाँठ है। अहंकार के किसी विचार के बिना, भगवत्-प्रीत्यर्थ कर्म करने से हम इस गाँठ को ढीली कर देते हैं और अंततः हम मुक्त हो जाते हैं।
अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार सभी कर्मों को यज्ञ-रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। यही यज्ञ के आरोहण की केंद्रीय चीज है। किस प्रकार व्यक्ति कोई भी कर्म अहं के लिये कर सकता है या फिर बुद्धि के विचार के अनुसार, सहजवृत्तियों के द्वारा, शरीर की वृत्तियों के द्वारा, या अकस्मात् यांत्रिक रूप से ही कर सकता है। आवश्यकता है कि उपरोक्त सभी कर्मों को यहाँ तक कि कुर्सी से उठने जैसे किसी छोटे-से-छोटे कर्म को भी भगवान् को अर्पित किया जाए। यह एक बड़ी महत् और उत्तरोत्तर वर्धमान चीज है। परंतु इसे लागू कैसे किया जाए? इसे लागू तो जो भी शक्ति हमें उपलब्ध है उसी के द्वारा करना होगा। हमारे अंदर जो भी शक्तियाँ हैं उन सभी को भगवान् की शक्ति के प्रति उत्सर्ग के रूप में मोड़कर यह लागू किया जा सकता है। हमारे ज्ञान के सभी कर्म, भक्ति के सभी कर्म, और संकल्प अथवा इच्छा-शक्ति के सभी कर्म, सभी को ही अर्पित कर देना होगा। अर्थात् हमारे समस्त ज्ञान को, सभी कुछ को उसी में लगा देना होगा। इसे लागू करने में बहुत सारी दुविधाएँ हैं, उन सभी का हमें सामना करना होगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर इतने तरीके के जाल बने हुए हैं, इतनी प्रकार की विषमताएँ हैं, संसार के विषय में अपने इतने दृष्टिकोण हैं जिनमें से किसी में भी हम फंसे हो सकते हैं, और उसी के अनुसार कर्म करने लगते हैं। क्योंकि इन सभी विषमताओं में प्रवृत्त करने वाली शक्तियाँ हैं जो हमें इनमें लगाए रखती हैं। मन के अपने सीधे-सादे सूत्र हैं जैसे कि 'कभी लालच लोभ मत करो', और यदि इन्हीं सूत्रों में व्यक्ति फंसा रहे तो पूरा आत्मोत्सर्ग कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि दिव्य जननी की महत् क्रिया कभी किसी भी सूत्र में सीमित नहीं हो सकती है। परंतु व्यक्ति शुरू में अपने तरह-तरह के सूत्रों के दृष्टिकोण से ही आरंभ करता है, परंतु यज्ञ के आरोहण में वह धीरे-धीरे सभी सूत्रों से परे निकल जाता है।
-------------------
* चलो... गीता के नियत कर्म को वैदिक प्रणाली का नित्यकर्म और उसके 'कर्तव्यं कर्म' को आर्य सामाजिक धर्म के रूप में मान लेते हैं और उसके 'यज्ञ रूप से किए गए कर्म' को वैदिक यज्ञ, एवं निःस्वार्थ भाव से तथा बिना किसी वैयक्तिक उद्देश्य के किया हुआ बँधा-बँधाया सामाजिक कर्त्तव्य मान लेते हैं। प्रायः गीता के निःस्वार्थ कर्म की इसी प्रकार व्याख्या की जाती है। परन्तु मुझे लगता है कि गीता की शिक्षा इतनी अनगढ़ और सहज नहीं है, इतनी देशकालमर्यादित और लौकिक तथा अनुदार नहीं है। यह तो उदार, स्वतंत्र, सूक्ष्म और गंभीर है; सब काल और सब मनुष्यों के लिये है, किसी काल विशेष और देश विशेष के लिये नहीं। विशेषतया, यह सदा बाहरी रूपों, ब्यौरों और सांप्रदायिक धारणाओं के बंधनों को तोड़कर मूल सिद्धान्तों की ओर तथा हमारे स्वभाव और हमारी सत्ता के महान् तथ्यों को और अपना रुख रखती है। गीता व्यापक दार्शनिक सत्य और आध्यात्मिक व्यावहारिकता का ग्रंथ है, अनुदार सांप्रदायिक और दार्शनिक सूत्रों और बँधे बँधाये मतवादों का ग्रंथ नहीं।
गीता यज्ञ का विस्तृत वर्णन करेगी कि वास्तव में इसका स्वरूप क्या है, इसका अर्थ क्या है। वह कहेगी कि सृष्टि के साथ-ही-साथ यज्ञ का विधान उसमें निहित है। हर चीज में परस्पर आदान-प्रदान चल ही रहा है और इसके द्वारा विकास चल रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कुछ दे न रही हो और जो स्वयं कुछ ग्रहण न कर रही हो। यही यज्ञ का सार्वभौम विचार है।
यद्यपि, आरम्भ में, गीता यज्ञ के विचार का वैदिक भाव ही लेती है और उस समय की प्रचलित वैदिक परिपाटी के अनुसार ही यज्ञ के विधान का वर्णन करती है, परंतु ऐसा यह एक सुनिश्चित उद्देश्य से करती है। हम लोग देख चुके हैं कि संन्यास और कर्म में जो झगड़ा है उसके दो रूप हैं; एक है सांख्य और योग का विरोध जिसका सिद्धांततः समन्वय इससे पहले किया जा चुका है, और दूसरा है वेदवाद और वेदांतवाद का विरोध जिसका समन्वय श्रीगुरु को अभी करना शेष है।.... वेदवाद यज्ञ के साथ देवताओं की पूजा करता और इन देवताओं को ऐसी शक्तियाँ मानता है जो हमारी मुक्ति में सहायता करती हैं। वेदांतवाद इन देवताओं को मानसिक और जड़प्राकृतिक जगत् की शक्तियों के रूप में मानने की ओर प्रवृत्त हुआ जिसके अनुसार देवता हमारी मुक्ति के विरोध में हैं (उपनिषद् कहते हैं कि मनुष्य देवताओं के पशु हैं, और देवता नहीं चाहते कि मनुष्य ज्ञानी और मुक्त हों), इसने भगवान् को अक्षर ब्रह्म के रूप में देखा है जिसे यज्ञकर्मों और उपासना के द्वारा नहीं, अपितु ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त करना होता है। (इसके अनुसार) कर्म तो केवल भौतिक फल और निम्न कोटि का स्वर्ग देनेवाले हैं, इसलिए कर्मों का त्याग करना ही होगा।
गीता इस विरोध का समाधान इस सिद्धांत के प्रतिपादन से करती है कि ये देवता एक ही परम् देव के, ईश्वर के, सब योगों, उपासनाओं, यज्ञों और तपों के परमेश्वर के ही केवल अनेक रूप हैं, और यदि यह सच है कि देवताओं को अर्पित किया हुआ हव्य केवल भौतिक फल और स्वर्ग को देनेवाला है, तो यह भी सच है कि ईश्वरप्रीत्यर्थ किया हुआ यज्ञ इनसे परे महान् मोक्ष तक ले जाने वाला होता है। क्योंकि परमेश्वर और अक्षर ब्रह्म दो भिन्न सत्ताएँ नहीं हैं, अपितु दोनों एक अभिन्न सत्ता हैं और इसलिए जो कोई इनमें से किसी को भी साधने का प्रयास करता है वह उसी एक भागवत् सत्ता को साधने का प्रयास करता है। अपनी समग्रता में सभी कर्म भगवान् के ज्ञान में अपनी पराकाष्ठा तथा परिसमाप्ति पाते हैं, 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते'। वे कोई बाधा नहीं हैं, अपितु परम् ज्ञान के मार्ग हैं। इस प्रकार इस विरोध का भी यज्ञ शब्द के अर्थ को व्यापक दृष्टि से सुस्पष्ट कर के समाधान किया गया है। वस्तुतः इसका विरोध योग और सांख्य का जो बड़ा विरोध है उसी का संक्षिप्त रूप है; वेदवाद योग का ही एक विशिष्ट और संकीर्ण रूप है; और वेदांतियों का सिद्धांत सांख्यों के सिद्धांत के तद्रूप ही है, क्योंकि दोनों के लिए ही मोक्ष प्राप्त करने की साधना है बुद्धि का प्रकृति की भेदात्मक शक्तियों से, अहंकार, मन और इन्द्रियों से तथा आंतरिक और बाह्य विषयों से निवृत्त होकर निर्विशेष और अक्षर पुरुष में वापस लौट आना। विभिन्न मतों का समन्वय साधने की इस बात को ध्यान में रखकर ही श्रीगुरु ने यज्ञविषयक अपने सिद्धांत के कथन का उपक्रम किया है; परन्तु इस सम्पूर्ण कथन में सर्वत्र, यहाँ तक कि एकदम आरंभ से ही, उनका ध्यान यज्ञ और कर्म के मर्यादित वैदिक अर्थ पर नहीं, अपितु उनकी उदार और व्यापक व्यवहार्यता पर रहा है, गीता की पद्धति सदा ही इन मतों की मर्यादित और बाह्य धारणाओं को विस्तृत करने और इन्होंने जिन महान् बहुप्रचलित सत्यों को सीमित रूप दे रखा है उन्हें उनके सत्य स्वरूप में प्रकट करने की रही है।
-------------
* आध्यात्मिक अर्थ में, 'सैक्रिफाइस' (त्याग, यज्ञ) का एक भिन्न अर्थ है - यह अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग को उतना सूचित नहीं करता जितना कि भगवान् के प्रति स्वयं अपने-आप के, अपनी सत्ता के, अपने मन, हृदय, संकल्प, शरीर, प्राण, कर्मादि के उत्सर्ग को सूचित करता है। इसका मूल अर्थ है 'पवित्र करना' और इसे 'यज्ञ' शब्द के पर्याय के रूप में प्रयोग किया गया है। जब गीता 'ज्ञान-यज्ञ' की बात कहती है तब उसका अर्थ किसी वस्तु का त्याग नहीं होता, अपितु उसका अर्थ होता है ज्ञान को खोज में मन को भगवान् की ओर मोड़ देना और उसके द्वारा अपने-आप को उत्सर्ग कर देना। फिर इसी अर्थ में व्यक्ति कर्मों के उत्सर्ग या यज्ञ की बात कहता है।... सैक्रिफाइस' शब्द का जो यूरोपियन अर्थ है वह 'यज्ञ' शब्द का अर्थ नहीं है या 'सैक्रिफाइस ऑफ वर्क्स' जैसे पदों में 'सैक्रिफाइस' का अर्थ यह नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान् के लिये तुम सभी कर्मों का त्याग कर दो - क्योंकि इसमें कर्मों का यज्ञ तो बिल्कुल होगा ही नहीं। इसी तरह ज्ञान-यज्ञ का अभिप्राय यह नहीं है कि तुम्हें कष्टपूर्वक और दृढ़ता के साथ परम प्रभु के लिये अपने-आप को मूर्ख बना देना होगा। 'सैक्रिफाइस' (यज्ञ) का तात्पर्य है भगवान् के प्रति आंतरिक दान, और एक यथार्थ आध्यात्मिक यज्ञ बहुत ही हर्षपूर्ण विषय है। अन्यथा व्यक्ति केवल अपने को योग्य बनाने का ही प्रयास कर रहा होता है और उसने अभी तक यथार्थ यज्ञ का प्रारंभ नहीं किया है।
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ।। १० ।।
१०. सृष्टि के प्रारम्भ में जीवों के पिता ने यज्ञ के साथ जीवों की सृष्टि कर के उनसे कहा इस यज्ञ के द्वारा तुम संतान या फलों को उत्पन्न करो, यह यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करनेवाला हो।
यज्ञ अर्थात् पारस्परिकता के विधान के द्वारा भगवान् ने तुम्हें सृष्ट किया है और इसी विधान के द्वारा तुम स्वयं वर्धित होओ, चीजों की उत्पत्ति करो और अपनी परिपूर्ति करो। क्योंकि यदि पारस्परिकता का विधान नहीं होता, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। प्रत्येक जीव, जिसे वह अपने से भिन्न मानता है, उससे कुछ-न-कुछ ग्रहण करता है और स्वयं भी समष्टि में कुछ-न-कुछ योगदान देता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे कि कोई भी प्रगति हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वह पत्थर हो, पौधा हो, पशु हो या मनुष्य हो, प्रत्येक ही हर समय कोई न कोई योगदान करता ही रहता है। भले व्यक्ति कोई विचार की धारा ही प्रदान कर रहा हो, पर तो भी समष्टि के अंदर योगदान करता अवश्य है। यह परस्परता यानि यज्ञ का विधान अधिरोपित किया गया था। क्योंकि, जब अहं आ जाता है, पृथक्ता का बोध आ जाता है, और तब यदि इस पारस्परिकता को उस पर न लादा गया होता, तो व्यक्ति कभी भूलकर भी इस विचार तक न आ पाता कि कोई एकात्मकता भी है, इस विचार तक कि ये सभी केवल बाह्य प्रतीतियाँ हैं, कि केवल एक ही परम् सत्ता, परमात्मा, जगज्जननी सर्वत्र ही व्याप्त हैं। इसलिए चूंकि इस बहुलता का (जो कि बाह्य दृश्यमान यथार्थता है) सृजन हुआ, और क्योंकि एकता वस्तुओं का निहित मूलभूत सत्य है, इसलिये सहज रूप से पारस्परिकता या यज्ञ-विधान दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की कड़ी का काम करता है। एकता और बहुलता दोनों ही पारस्परिकता के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब चूंकि वास्तव में तो एकता और बहुलता मूलभूत रूप से एक ही हैं इसलिये उनके बीच यज्ञ-विधान तो अवश्यंभावी हो ही जाता है। जिस प्रकार एक ही देह में सर्वत्र ही रक्त का संचार होता है और अंगों में पारस्परिक आदान-प्रदान होता है उसी प्रकार यहाँ भी है। इस आदान-प्रदान से हम अपनी व्यष्टि सत्ता, फिर वैश्विक सत्ता और तब फिर परात्पर सत्ता के, चेतना के इन तीनों स्तरों के विषय में सचेतन होते हैं।
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।। ११ ।।
११. इस यज्ञ द्वारा तुम देवों को पुष्ट करो, और वे देव तुम्हारा पोषण करें; इस प्रकार एक दूसरे का पोषण-वर्धन करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त कर लोगे।
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ।। १२ ।।
१२. यज्ञ से संपुष्ट हुए देव तुम्हें निश्चय ही अभीष्ट भोग्य पदार्थों को प्रदान करेंगे; जो मनुष्य उनसे प्रदत्त भोग्य पदार्थों को उन्हें न देकर स्वयं भोग करता है वह चोर है।
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
भुञ्जते ते त्वषं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ।। १३ ।।
१३. जो सत् पुरुष यज्ञ से बचे हुए अंश को खाते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं; परंतु जो केवल अपने लिये ही भोजन पकाते हैं वे पापी होते हैं और पाप का भक्षण करते हैं।
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।। १४ ।।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।। १५।।
१४-१५. अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है; कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है; इसलिये सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है।
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ।। १६।।
१६. हे पार्थ! जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार प्रवृत्त किये हुए चक्र का अनुसरण नहीं करता वह पापमय जीवनवाला है, इन्द्रियों के विषयों में रमण करता है, वह व्यर्थ ही जीता है।
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।। १७।।
१७. परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा के स्वरूपभूत आनंद में तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिये कोई कर्त्तव्य कर्म (ऐसा कर्म जिसे करने की आवश्यकता रह गयी हो अथवा जिसे करना आवश्यक हो) नहीं रहता।
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।
न चास्य सर्वभूतेषु कश्विदर्थव्यपाश्रयः ।।१८।।
१८. इस संसार में उसे कर्म करने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है और न ही न करने से कोई पदार्थ प्राप्त करना है; उसे इन समस्त भूतों पर किसी प्राप्त होने योग्य पदार्थ के लिये आश्रित नहीं होना पड़ता है।
उपरोक्त सब के अंदर हमें इनके पीछे के रूपक को समझने का प्रयास करना चाहिये। गीता के अंदर हमें विचारों को सतही तौर पर न लेकर उन्हें उनकी चरम गहराइयों में देखना चाहिये। तब वे अपना सच्चा स्वरूप और औचित्य अपना लेते हैं क्योंकि वही उनका अभिप्रेत अर्थ है, न कि सतही। इसमें पहला श्लोक कि 'यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो' इसमें यज्ञ का जो विचार है, उसके पीछे जो निहित कारण है वह कोई चयन का विषय नहीं है (अर्थात् इसमें कोई व्यक्तिगत चयन निहित नहीं है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से यज्ञ के विधान को अपना या नकार सकता हो) बल्कि यह तो सारे ब्रह्माण्ड के एकत्व की एक मूलभूत स्थिति है। केवल 'एकमेवाद्वितीयम्' का ही अस्तित्व है, उसी की सत्ता है। यदि बहुलता का सृजन हुआ है तो यह केवल एक प्रतीति मात्र है, वास्तव में तो कोई विभाजन है ही नहीं और विभाजन संभव भी नहीं है। प्रतीति में भी जो बहुलता है उसमें भी पारस्परिक आदान-प्रदान का विधान निहित है। जैसे कि, यदि हम व्यक्ति के शरीर में प्रत्येक कोशिका को अपने-आप में एक अलग इकाई मान लें, तो भी उनमें आपस में परस्पर आदान-प्रदान होता ही है, इसी कारण मनुष्य का शरीर बना रहता है अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी है वह सभी भगवान् के दिव्य शरीर की कोशिकाएँ हैं और 'उनमें' वे सब एक हैं। इसलिए पारस्परिक आदान-प्रदान होता है। परन्तु वे कोशिकाएँ जो सदा प्राप्त ही करना चाहती हैं, देना नहीं चाहती, वे शरीर में कैंसर की तरह हैं। तो पहली चीज है ब्रह्माण्ड का यह एकत्व जो यज्ञ के सिद्धान्त को बाध्यकारी बना देता है, इसमें कोई चयन का विषय नहीं रह जाता। यदि कोई इकाई अपने को उस प्रवाह से अलग समझे, फिर चाहे वह व्यक्ति हो, समुदाय हो, समाज हो, देश हो या फिर मानवजाति ही क्यों न हो, तो वह कैंसर के समान है। क्योंकि ये सभी तो उस एक ही सत्ता के शरीर की कोशिकाएँ हैं। इसलिए इसे स्वीकार करो या न करो, यह तो बाध्यकारी है ही। यदि व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करता तो उसे इस सचेतन यज्ञ का मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त नहीं होता। प्रकृति बाध्यकारी रूप से यह यज्ञ करवाती ही है। भले कोई यज्ञ के लिये या फिर प्रदान करने के लिए कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो परन्तु उसे यज्ञ करना हो होगा, शक्तियों का आदान-प्रदान करना ही होगा।
तो इस श्लोक के प्रतीक में चलें कि 'यज्ञ के द्वारा संतान की या फिर अभीष्ट फलों की उत्पत्ति होती है।' जो व्यक्ति आदान-प्रदान नहीं करता वह कभी भी स्वयं को निरंतर नहीं रख पाएगा, अपने को बनाए नहीं रख पाएगा, अर्थात् अपनी संतति की उत्पत्ति नहीं कर सकता, कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। केवल इसी के द्वारा व्यक्ति अपने आप को संतति के रूप में तथा अन्य चीजों के रूप में, प्रभावों और फलों के रूप में उत्पन्न कर सकता है।
दूसरा श्लोक है कि 'इस यज्ञ द्वारा देवों को पुष्ट करो और देव ही तुम्हारा पोषण करेंगे। और इसके द्वारा एक-दूसरे का भरण पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त कर लोगे।' इसमें तो वेद का सारा सार ही आ गया कि किस प्रकार परस्पर आदान-प्रदान करते हुए मनुष्य अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों को अधिकाधिक पुष्ट करता जाता है। इन मनोवैज्ञानिक शक्तियों के रूप में देवता अभिव्यक्त होते हैं और ये सारा ब्रह्माण्ड देवताओं के द्वारा ही निर्मित है। मनुष्यों की सारी मनोवैज्ञानिक शक्तियों और इन्द्रियों के पीछे देवता ही हैं। व्यक्ति इन्द्रियों के माध्यम से इस जगत् को देखता है, क्योंकि वास्तव में तो कुछ है ही नहीं और क्या है या नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे लिए तो यह सब इंद्रियों के द्वारा रचा जाता है। व्यक्ति का इंद्रिय बोध उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। इंद्रियाँ वही होते हुए भी यदि मानसिकता एक बिल्ली की होगी तो व्यक्ति क्या बोध प्राप्त करेगा, और चूहे की होगी तो और भी भिन्न बोध प्राप्त करेगा। इस प्रकार इस श्लोक में गीता कह रही है कि यदि व्यक्ति ने पारस्परिक आदान-प्रदान के द्वारा अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों और इन्द्रियों की वृद्धि की दिशा में कुछ काम किया है तो अवश्य ही उन्हें पुष्ट कर सकता है, अन्यथा नहीं। यदि व्यक्ति ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया है तो वह असंस्कृत रह जाएगा। मनुष्यों में तो यह संवर्धित करने की संभावना होती है अन्यथा संस्कारित करने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसके बिना तो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को ही संतुष्ट करने में लगा रहता है जैसे कि एक पशु इसमें लगा रहता है। तो इसमें तो कोई नयी रचना होगी नहीं। मनुष्य में यह संभावना है कि वह आदान-प्रदान के द्वारा अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों को विकसित करे तो इससे एक नयी रचना होगी। यदि मनुष्य में ये शक्तियाँ विकसित नहीं हुई होतीं तो भौतिक जगत् की भी दशा, उसकी स्थिति जैसी आज है वैसी नहीं होती। इससे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है और ज्यों-ज्यों व्यक्ति आदान-प्रदान करेगा त्यों-ही-त्यों अंततः वह चरम स्थिति तक पहुँच जाएगा। मनुष्य तो अभी बड़ी ही असंस्कृत अवस्था में है जहाँ वह केवल अपनी इन्द्रियों के विषयों आदि के आदान-प्रदान पर ही केंद्रित है।
इसके बाद जब व्यक्ति के अंदर विचार उठते हैं, तो ये हैं मरुद्गण। व्यक्ति की भावनाओं से जब विचार पैदा होते हैं कि 'ऐसा करना चाहिये, यह सही है, यह गलत है' या फिर यदि किसी के समझ में आ गया हो कि यह सब तो बेकार है, तब वह अपने सारे जीवन में अनुशासन लाकर उससे परे निकल जाता है। यह मरुद्गणों की क्रिया का प्रभाव है। उसके बाद जब वह और आगे चलता है तो उसकी और शक्तियाँ भी विकसित होती जाती हैं। फिर वह परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और उसमें इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं कि वह उन्हें ग्रहण कर के महत् सृजन कर सकता है क्योंकि अन्दर निहित शक्तियों का कोई अंत नहीं होता। यही वेदों का रहस्य है, कि व्यक्ति अपनी मनोवैज्ञानिक अथवा अध्यात्मपरक शक्तियों को पुष्ट करे और तब फिर वह उन शक्तियों के द्वारा शक्तिशाली रूप से क्रिया कर सकता है। हमारी मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ यदि शक्तिशाली हों तो हम बड़े ही सशक्त रूप से क्रिया कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे ऋषि कितनी शक्तिशाली रूप से क्रिया कर सकते थे। इस प्रकार व्यक्ति यह कार्य कर के अपने जीवन को, अभिव्यक्ति को बहुत अधिक प्रचुर और समृद्ध बना सकता है। यही इन सब बातों का अर्थ है। इसमें वेदों की सारी कुंजी ही निहित है। मनुष्य के मनोविज्ञान के पीछे भी देवता हैं और उससे स्वतंत्र भी हैं। और जब व्यक्ति उन तक पहुँच जाएगा तब ये मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ भी अपने पूरे वैभव को प्राप्त कर लेंगी। पहले तो ये देवता मनुष्य की सीमित मानसिकता में सीमित क्रिया ही करते हैं। परन्तु जब व्यक्ति किसी एक स्तर-विशेष से ऊपर उठ जाता है, जब मरुद्गणों के बाद इन्द्र की क्रिया शुरू हो जाती है तब मनुष्य के अनचाहे प्राणिक और भौतिक हस्तक्षेप समाप्त हो जाते हैं और इसके बाद वह बहुत विशाल निर्माण कर सकने की स्थिति में होता है। जब वह और ऊपर उठता है तो देवताओं की खुले तौर पर क्रिया प्रारम्भ हो जाती है और उससे तो भगवद्-प्रेरित निर्माण कर सकने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन्होंने भी कोई महान् कार्य किए हैं उन्होंने इसी प्रकार से एक-एक क्षेत्र में अद्भुत निर्माण किया है। श्रीअरविन्द के अनुसार वेदव्यास, वाल्मीकि और कालीदास, इन तीनों ने तो सारे भारतवर्ष का ही निर्माण कर दिया। उन्होंने उन चीजों को अभिव्यक्ति प्रदान की जिनसे सब चीजों का निर्माण हुआ और आज भी हमारी सारी संस्कृति उनसे प्रेरित है। इससे निर्माण बहुत ही विशाल बन गया, इसी को सूत्र रूप में अगले श्लोक में बताया गया है।
"यज्ञ से संपुष्ट हुए देव तुम्हें निश्चय ही अभीष्ट भोग्य पदार्थों को प्रदान करेंगे; जो मनुष्य उनसे प्रदत्त भोग्य पदार्थों को उन्हें न देकर स्वयं भोग करता है वह चोर है।" इस परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया में जब मनुष्य अपने जीवन में देवों को उतरने देता है और उनसे जो शक्ति-सामर्थ्य विकसित होते हैं तो उससे जड़तत्त्व पर अधिक नियंत्रण करने की शक्तियाँ आ जाती हैं, परंतु जब व्यक्ति इन्हें अपने अहं की तुष्टि के लिए उपयोग करता है, इन शक्तियों को और ऊपर उठने का एक माध्यम न बनाकर अहं की तुष्टि में लग जाता है तो इसका अर्थ है कि उसने यज्ञ मार्ग को छोड़ दिया है और पथ से भ्रष्ट हो गया है। क्योंकि जो भी शक्ति उसने उस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की उसे उसने निम्न प्रकृति को अर्पण कर दिया है तो इसका अर्थ है कि वह आगे न जाकर रास्ते से भटक गया। अतः इससे व्यक्ति को बचना चाहिए।
"जो सत् पुरुष यज्ञ से बचे हुए अंश को खाते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं, वे पापी होते हैं, और पाप का भक्षण करते हैं।" इस श्लोक में गीता इसी बात को और अधिक बल के साथ कह रही है कि यज्ञ करने में मनुष्य ने जो प्रयत्न लगाए उन्होंने उसे पवित्र बना दिया। यज्ञ के बाद बचा हुआ भाग भगवान् शंकर का भाग बताया जाता है जो कि परात्पर भगवान् हैं। वे सारे ब्रह्माण्ड से परे हैं, यज्ञ के बाद बचा हुआ भाग उन्हीं का है। कहने का वास्तव में अर्थ यह है कि यज्ञ में अर्पित करने के बाद भी व्यक्ति में इतनी शक्तियाँ फिर भी बची रह जाती हैं जिन्हें वह स्वयं में स्थित परात्पर को अर्पित करता है।
"अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है। यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म, सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है।" इसमें भौतिक रूप से तो वृष्टि का अर्थ स्पष्ट ही है परन्तु वैदिक प्रतीक के अनुसार वृष्टि का अर्थ है भागवत् कृपा का अवतरण जिसके द्वारा व्यक्ति को जो चीजें पहले स्पष्ट नहीं थीं वे स्पष्ट हो जाती हैं और जो काम वह पहले नहीं कर पाता था उन कामों को करने में वह सक्षम हो जाता है। इस कृपा से मनुष्य के (सभी अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोष) अर्थात् शरीर, प्राण और मन पुष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को अपनी सारी सत्ता का आधार उसमें मिल जाता है। इस प्रकार कृपा के रूप में वृष्टि आती है। वृष्टि यज्ञ का परिणाम है। जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो प्रसन्न होकर देवता वृष्टि (कृपा) करते हैं। वेदों में इस प्रतीक का बार-बार में वर्णन है कि स्वर्ग के जलों का अवतरण होता है। और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य कर्म नहीं करता तो यज्ञ हो हो नहीं सकता। जब हम हमारे मन, प्राण शरीर के समस्त कर्मों को अग्नि को समर्पित करते हैं तब वह यज्ञ होता है और हमारे समस्त कर्म, विचार, भावनाएँ हमारे भीतर स्थित ब्रह्म से, अन्तरात्मा से उत्पन्न होते हैं, यह सारी प्रतीति ब्रहा है जो अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होती है और इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। क्योंकि सभी कुछ का आरम्भ वहीं से होता है। भगवान् स्वयं ही यज्ञ करते हैं, स्वयं ही यज्ञ हैं और स्वयं ही यज्ञ को ग्रहण करते हैं। इसका चतुर्थ अध्याय में निरूपण होगा। अतएव मनुष्य के यज्ञ कर्म में परमात्मा सदा ही सम्मिलित हैं। क्योंकि उन्हीं से समस्त कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्मों से यज्ञ और फिर यज्ञ से वृष्टि, भागवत् कृपा, अवतीर्ण होती है जिससे सभी कुछ फलीभूत होता है।
हे पार्थ! जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार प्रवृत्त किये हुए चक्र का अनुसरण नहीं करता वह पापमय जीवन वाला है, इन्द्रियों के विषयों में रमण करता है, वह व्यर्थ ही जीता है। जो मनुष्य इस आदान-प्रदान की क्रिया को अर्थात् यज्ञ को न कर के, भगवद्-संकल्प अर्थात् अग्नि के अन्दर कोई होम नहीं करता और केवल पणियों और वृत्रों को ही भेंट करता है, वह पापमय जीवन ही जीता है। इस दृष्टिकोण से अधिकांश मनुष्यों का जीवन पापमय ही है इसलिए इसके परिणाम भी पापमय ही हैं क्योंकि आत्मोत्सर्ग तो है ही नहीं। इसी को पापमय जीवन बताया गया है। क्योंकि यहाँ जो कुछ भागवत् कृपा के परिणाम से मिलता है, उसको मनुष्य विराधी शक्तियों को (अर्थात् पणियों को या वृत्रों को, अपने अहं की शक्तियों को) भेंट कर देता है।
"परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा के स्वरूपभूत आनंद में तृप्त रहता है, और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्त्तव्य कर्म नहीं रहता।" अब यहाँ कर्तव्यं कर्म कहा गया है, तो यह कर्तव्यं कर्म व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गठन से निर्धारित होता है कि कौनसा कर्म करना चाहिये और कौनसा नहीं करना चाहिये। जो मनुष्य परमात्मा से एकमय हो गया है उसे किन्हीं बाहरी मापदण्डों की आवश्यकता नहीं रहती। वह तो हमेशा ही आनन्द में रहता है। उसे कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। वह तो केवल भागवत्-संकल्प अथवा भगवद्-इच्छा के अनुसार कर्म करता है और प्रायः बहुत घोर कर्म करता है, अकर्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अतः, जो व्यक्ति ब्रह्म से जुड़ जाता है उस पर कर्म करने के या न करने के कोई बाहरी मापदण्ड नहीं लगाए जा सकते और न ही उनका कोई अर्थ है। इस रूप में हम इसे देख सकते हैं। वेद के इस रूपक में और अधिक गहराई में जाया जा सकता है परंतु वर्तमान के लिये इतना समझ लेना पर्याप्त होगा।
जो मनुष्य जगदम्बा से युक्त हो जाता है उस पर कोई बाहरी मापदण्ड लागू नहीं होते। निष्काम कर्म आदि के मापदण्ड तो विकसित होते जीव पर ही लागू होते हैं। जो भागवत् संकल्प से जुड़ गया है, जो श्रीमाताजी के साथ जुड़ गया है उसके कर्म तो उन्हीं से निर्देशित होते हैं, इसलिए उस पर कर्म-अकर्म के कोई भी मानवीय मापदण्ड लागू नहीं होते।
"इस संसार में उसे कर्म करने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है और न ही न करने से कोई पदार्थ प्राप्त करना है। उसे इन समस्त भूतों पर किसी प्राप्त होने योग्य पदार्थ के लिए आश्रित नहीं होना पड़ता।" कर्म-अकर्म से ऐसे मनुष्य को कोई लेना देना नहीं है। वह तो इस सब से ऊपर उठ जाता है।
यहाँ दो भिन्न आदर्श, - वेदवादी और वेदांतवादी - उपस्थित हैं मानो दोनों अपने मूलगत परस्पर-पार्थक्य और विरोध को लिये हुए खड़े हैं। एक ओर है वेदवादी का यज्ञ के द्वारा और मनुष्यों तथा देवताओं के परस्पर-आश्रय के द्वारा इहलोक में सांसारिक भोगों और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति का सक्रिय आदर्श, और उसी के सामने दूसरा है उस मुक्त पुरुष का कठोरतर (वेदांतवादी) आदर्श जिसका आत्मा के स्वातंत्र्य में स्थित होने के कारण भोग से या कर्मों से अथवा मानव-जगत् से या दिव्य जगतों से कोई लेना-देना नहीं, जो केवल परम् आत्मा की शांति में निवास करता है और ब्रह्म के प्रशांत आनन्द में आनंदित होता है। इसके आगे के श्लोक इन दो चरम पंथों के बीच समन्वय साधने के लिये भूमिका तैयार करते हैं; इस समन्वय का रहस्य यह है कि उच्चतर सत्य की ओर अभिमुख होते ही अकर्म नहीं, अपितु निष्काम कर्म है जो उस सत्य की उपलब्धि के पहले और पीछे भी वांछनीय है। मुक्त पुरुष को कर्म के द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं करना, परंतु अकर्म से भी उसे कोई लाभ नहीं उठाना; और उसे जो अपना चयन करना है वह बिल्कुल भी किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के अनुसार नहीं होता ।...
इस शिक्षा का संपूर्ण अर्थ और भाव व स्वरूप हम यज्ञ, कर्म और ब्रहा, इन महत्त्वपूर्ण शब्दों की जैसी व्याख्या करते हैं उसी के अनुरूप हो जाता है। यदि यज्ञ का अर्थ केवल वैदिक यज्ञ ही हो, यदि जिस कर्म से यह यज्ञ उत्पन्न होता है वह वैदिक कर्मविधि ही हो और यदि वह ब्रह्म जिससे समस्त कर्मों का उद्भव होता है वह वेदों की शब्दराशिरूप शब्दब्रह्म ही हो तो वेदवादियों के सिद्धान्त की सब बातें स्वीकृत हो जाती हैं और कुछ नहीं रह जाता। आनुष्ठानिक यज्ञ संतति, संपत्ति और भोग की प्राप्ति का उचित साधन है... यहाँ तक कि मोक्ष भी, परम कल्याण भी, आनुष्ठानिक यज्ञ से प्राप्त होना है। इसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिये। यहाँ तक कि मुमुक्षु को भी आनुष्ठानिक यज्ञ करते रहना होता है, यद्यपि आसक्ति-रहित होकर; आनुष्ठानिक यज्ञों और शास्त्रोक्त कर्मकाण्डी कर्मों को निर्लिप्त भाव से करने से ही जनक जैसों को आध्यात्मिक पूर्णता और मुक्ति प्राप्त हुई।
स्पष्टतः ही, गीता का यह अभिप्राय नहीं हो सकता; क्योंकि यह ग्रंथ की शेष सारी शिक्षा के विपरीत होगा। चौथे अध्याय में यज्ञ की दी गई जो उद्बोधक व्याख्या है उसके बिना भी, इस वर्तमान भाग में ही हमें पहले ही इसके व्यापक अर्थ का संकेत प्राप्त होता है जहाँ यह कहा गया है कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म ब्रह्म से ब्रह्म अक्षर से, और इसलिए सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर 'इसलिए' शब्द का संयोजक संबंध और 'ब्रह्म' शब्द की पुनरुक्ति का विशेष अर्थ है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस ब्रह्म से सब कर्म उत्पन्न होते हैं उस ब्रह्म को हमें प्रचलित वेदवादियों के शब्दब्रह्म के अर्थ में नहीं, अपितु वेद का रूपकात्मक अर्थ कर के सर्जनकारी शब्द को सर्वगत ब्रह्म के साथ, शाश्वत पुरुष के साथ, सब भूतों में जो एक आत्मा है उसके साथ तथा समस्त भूतों की क्रियाओं के अन्दर प्रतिष्ठित जो ब्रह्म है उसके साथ, एक समझना होगा।... प्रकृति की समस्त क्रिया ही, अपने वास्तविक स्वरूप में एक यज्ञ है जिसमें दिव्य पुरुष सभी तपों, कर्मों और यज्ञ के भोक्ता हैं और सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, 'भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्'। और, इन भगवान् को, जो सर्वगत हैं तथा यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं, 'सर्वगतं यज्ञे प्रतिष्ठितं', जानना ही सच्चा ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है।
iii. 20, v.29
यह एक मूलभूत तथ्य है। यहाँ इस ब्रह्माण्ड में (The Two who are one are the might and right in things. - Savitri, p. 63) परम प्रभु स्वयं ही अपने दो रूपों में विद्यमान हैं - परम प्रभु स्वयं और उनकी चित्-शक्ति। तीसरा कोई है ही नहीं। ये जो भी रूप हैं वे सारे ब्रह्म के ही रूप हैं। उन्हीं की चेतना उन सब के साथ कार्य-व्यवहार करती है। परमात्मा के आनन्द के लिए ही यह सारा काम हो रहा है। इस दृष्टिकोण के अतिरिक्त अन्य किसी दृष्टिकोण से तो हम सच्चे रूप में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब व्यक्ति चेतना के इस प्रवाह में अहं का कोई स्पंदन पैदा करता है, अपने शरीरादि के आनंद के लिए कोई अहंपरक स्पंदन पैदा करता है तब वह यह भूल जाता है कि परा-प्रकृति यह सारा व्यापार उसके अहं के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के आनंद के लिये करती है, और इसी कारण व्यक्ति को थपेड़े पड़ते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति स्वयं की तुष्टि के लिए काम करेगा, उसकी दुर्गति होगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि न हो क्योंकि वह ऐसे बहाव को मोड़ने का प्रयास कर रहा होता है जिसे मोड़ने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। क्योंकि वह तो पराशक्ति है। परन्तु वह शक्ति साथ-ही-साथ हमारी चेतना को बढ़ाने का काम भी करती है इसलिए वह हमारी इन सब चीजों को अपनी लहरों के उतार-चढ़ावों में सहन करती है। परंतु इस भागवत्-संकल्प के विरुद्ध जाकर हम कभी भी कोई कल्याणकारी चीज नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि इस भागवत्-संकल्प का कार्य है सभी कुछ को यज्ञ रूप में परम प्रभु को समर्पित करना।
परन्तु इन भगवान् को देवताओं, अर्थात् प्रकृतिस्थ दिव्य पुरुष को शक्तियों, के द्वारा होती इससे एक निम्नतर कोटि की क्रिया में तथा इन शक्तियों के मानव की आत्मा के साथ होने वाले शाश्वत संसर्ग में जाना जा सकता है जिसमें ये देवता और मानव आत्मा परस्पर एक दूसरे को दान देते हैं और प्रतिदान में प्राप्त करते हैं, एक दूसरे की सहायता और संवर्धन करते हैं, और एक दूसरे की क्रिया और तुष्टि को बढ़ाते हैं, यह एक ऐसा दान-प्रतिदान है जिसमें मनुष्य परम कल्याण का अधिकाधिक अधिकारी होता जाता है। वह यह अनुभव कर लेता है कि उसका जीवन प्रकृति में इस परम् पुरुष की दिव्य क्रिया का एक अंग है, न कि इससे कोई पृथक् चीज है जिसको कि उसकी अपनी तुष्टि के लिए ही धारण करना या निर्वाह करना हो। वह अपने भोगों को और कामनाओं की तुष्टियों को यज्ञ के फल और दिव्य वैश्विक क्रियाओं में रत देवताओं की देन के रूप में मानता है। और, वह पापमय अहंकारपूर्ण स्वार्थपरता - जिसके अनुसार इन भोगों और तुष्टियों को (देवताओं की सहायता के बिना) स्वयं अपने बल पर ही छीना जा सकता है और जिनका प्रतिदान या आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं- के मिथ्या और दुष्ट भाव से प्रेरित होकर उन भोगों का पीछा करना छोड़ देता है। ज्यों-ज्यों यह भाव उसमें बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों वह अपनी इच्छाओं को गौण व अधीन करता जाता है, जीवन और कर्मों के विधान के रूप में यज्ञ को जानकर संतुष्ट हो जाता है और यज्ञावशेष को ही पाकर परितृप्त हो जाता है, शेष सब कुछ को अपने जीवन और जगत्-जीवन के बीच परस्पर होने वाले महान् और परम हितकर आदान-प्रदान पर मुक्त रूप से न्यौछावर कर देता है। जो कोई कर्म के इस विधान के विरुद्ध जाता है और अपने ही पृथक् व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर्मों और भोगों में लिप्त रहता है वह व्यर्थ ही जीता है; वह जीवन के वास्तविक अर्थ और उसके उद्देश्य और उसकी उपयोगिता से तथा जीव की ऊर्ध्वगति से वंचित रहता है; वह उस मार्ग पर नहीं है जो परम कल्याण की ओर ले जाता है। परन्तु परम पद की प्राप्ति तब होती है जब यज्ञ देवताओं के लिए नहीं, अपितु उन सर्वगत परमेश्वर के लिए किया जाता है जो यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं, देवता जिनके कनिष्ठ रूप और शक्तियाँ हैं, और जब व्यक्ति अपने निम्नतर स्वत्व को छोड़कर, जो कामना और भोग में रत है, स्वयं के कर्ता होने के बोध को त्याग देता है और सभी कर्मों की वास्तविक कर्ती, प्रकृति, को मानने लगता है तथा अपने स्वयं भोक्ता होने के भाव को दिव्य पुरुष को, उस उच्चतर और विश्वात्मा को सौंप देता है जो कि प्रकृति की क्रियाओं का वास्तविक भोक्ता है। उसी आत्मा में, न कि किसी व्यक्तिगत भोग में, उसे अपना एकमात्र संतोष, पूर्ण तृप्ति और विशुद्ध आनन्द प्राप्त होता है; उसे अब कर्म या अकर्म से कोई लाभ नहीं, वह किसी भी चीज के लिए न देवताओं पर आश्रित है न मनुष्यों पर, किसी से किसी लाभ की अभिलाषा नहीं रखता; क्योंकि स्वात्मानन्द ही उसके लिए सर्वथा पर्याप्त है; परन्तु फिर भी वह केवल भगवान् के लिए, आसक्ति या कामना से रहित होकर शुद्ध यज्ञरूप से कर्म करता है। इस प्रकार वह समत्व को प्राप्त होता और प्रकृति के त्रिगुण से मुक्त हो नित्रैगुण्य हो जाता है; जब उसके कर्म प्रकृति की कर्मधारा में जारी भी रहते हैं तब भी उसकी आत्मा प्रकृति की अनिश्चितता में नहीं, अपितु अक्षर ब्रह्म की शांति में स्थित होती है। इस प्रकार यज्ञ परमपद की प्राप्ति में उसका साधन-मार्ग होता है।
यज्ञसंबंधी इस प्रकरण का यही अभिप्राय है ऐसा इसके आगे जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है, अर्थात् लोक-संग्रह को कर्मों के ध्येय के रूप में स्थापित कर के, प्रकृति को ही कर्मों की एकमात्र कर्मी बताकर और दिव्य पुरुष को उन सब कर्मों का समान भर्त्ता बताकर, जिसे कि सभी कर्म, उन कर्मों के होते समय भी, अर्पण करने होते हैं- यह आंतरिक रूप से सब कर्मों का त्याग करना और फिर भी भौतिक रूप से कर्म को करते रहना ही यज्ञ की परिसमाप्ति है, तथा यही अभिप्राय है ऐसा इस अभिपुष्टि से भी स्पष्ट हो जाता है कि सम और निष्काम बुद्धि से इस प्रकार जो कर्ममय यज्ञ किया जाता है उसका फल कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है।
iii 27, iii. 30, iv. 23
इसमें मुख्य बात है मनुष्यों और देवताओं के बीच होने वाला आदान-प्रदान। परन्तु देवताओं से अभिप्राय प्रचलित तौर पर हम जिन्हें देवता कहते हैं उनसे नहीं है और आदान-प्रदान का अर्थ यह नहीं कि कोई मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा-पाठ करने या प्रसाद आदि चढ़ाने की बात हो। इस प्रकार के आदान-प्रदान को सच्चा यज्ञ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देवता तो व्यक्ति के अंदर उसकी विभिन्न मनोवैज्ञानिक शक्ति-सामर्थ्य के रूप में प्रकट रहते हैं, वे अध्यात्मपरक शक्तियाँ हैं। जब व्यक्ति अपने-आप को इन शक्तियों के अधीन रखकर उनके अंतर्गत काम करता है तब इसका अर्थ है कि वह उन देवताओं को भेंट अर्पित कर रहा है। जब व्यक्ति मानसिक या प्राणिक आदर्श के लिए काम करता है तब उनके पीछे स्थित मनोवैज्ञानिक या फिर अध्यात्मपरक देवताओं को वह अपनी शक्ति-सामर्थ्य भेंट करके पुष्ट करता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन को किसी आदर्श या मत-विशेष के लिए समर्पित कर देता है। जैसे गीता में भगवान् कहते हैं कि जो मनुष्य भूतों के लिए यज्ञ करते हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं, यक्षों की पूजा करने वाले यक्षों को, पितरों को पूजा करने वाले पितरों को, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को और मेरी पूजा करने वाले मेरे को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति के अंदर भौतिक, प्राणिक, मानसिक जो विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं उनके पीछे सूक्ष्म सत्ताएँ होती हैं। जब व्यक्ति अपनी प्राणिक इच्छाओं, कामनाओं और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की चेष्टा करता है तब इसका अर्थ है कि वह केवल उन प्राणिक सत्ताओं के लिए ही कर्म करता है जिन्हें यक्ष, गन्धर्व, राक्षस आदि की संज्ञा दी गई है और उनसे व्यक्ति को जीवन में जो मिलता है वह तो स्पष्ट ही है। और जब व्यक्ति उन सत्ताओं को जीवन में और अधिक स्थान देता है तो, धीरे-धीरे वे व्यक्ति के जीवन पर अधिकार कर लेते हैं जिससे जीवन में और कुछ नहीं बचता। तो मनुष्य धीरे-धीरे यह सीखता है कि ये सही चीजें नहीं हैं। यदि मनुष्य या समाज का कोई आदर्श नहीं है तो ऐसा मनुष्य या ऐसा समाज पशुतुल्य ही है। क्योंकि इस तरीके के काम तो पशु भी करते हैं। जब व्यक्ति किसी आदर्श के लिए प्रयत्न करता है- फिर वह चाहे बहुत निम्न कोटि का ही क्यों न हो - तो वह कुछ अधिक ऊपर के देवताओं का अनुसरण कर रहा होता है और तब भौतिक कामनाओं और वासनाओं में ही घोर रूप से लिप्त रहने की बजाय उसमें कुछ सुधार आता है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो थोड़ा-बहुत सुसंस्कृत हो पर यह न सोचे कि यह घोर लिप्तता तो ठीक नहीं है? इस संस्कार के बिना तो मनुष्य केवल निम्न सुख की ही लालसा करता है और किन्हीं श्रेष्ठतर चीजों से उसे कोई मतलब नहीं होता। जब व्यक्ति अपने-आप को विभिन्न प्रेरणाओं के प्रति या विभिन्न देवताओं (अर्थात् विभिन्न मनोवैज्ञानिक शक्तियों) के प्रति समर्पित करता है - क्योंकि हर एक का अपना-अपना आदर्श होता है - और उन्हें अपने जीवन में प्रयुक्त करता है तब वह उस शक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान करता है।
--------------------
* करणीय कर्म को सूचित करने के लिये गीता में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसकी व्याख्या अवश्य ही इस अर्थ में की गई है कि हमें फल का विचार किये बिना अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिये। किन्तु यह एक ऐसी धारणा है जो यूरोपीय संस्कृति की उपज है जो आध्यात्मिक की अपेक्षा कहीं अधिक नैतिक है और अपनी अवधारणा में आंतरिक रूप से गंभीर होने की अपेक्षा कहीं अधिक बाह्य है। कर्त्तव्य जैसी किसी सामान्य बाह्य वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है; हमारे सामने तो केवल कर्त्तव्य होते हैं जो प्रायः परस्पर विरोधी होते हैं। ये कर्तव्य हमारे परिवेश, हमारे सामाजिक सम्बन्धों और हमारी बाह्य जीवन-स्थिति से निर्धारित होते हैं। अपरिपक्व नैतिक प्रकृति को सुधारने तथा स्वार्थपूर्ण कामना के कर्म को निरुत्साहित करने वाले प्रतिमान की स्थापना करने में ये भारी महत्त्व के हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जब तक अभीप्सु के पास कोई आन्तरिक प्रकाश नहीं होता तब तक उसे उस सर्वोत्तम प्रकाश के अनुसार ही चलना होगा जो उसे उपलब्ध है; और इसमें कर्तव्य, कोई सिद्धान्त, कोई निमित्त या ध्येय उन प्रतिमानों में से हैं जिनकी वह कुछ काल के लिए स्थापना तथा अनुसरण कर सकता है। परन्तु यह सब होते हुए भी, कर्तव्य कर्म बाह्य चीजें हैं, आत्मा की वस्तु नहीं और ये इस पथ में कर्म के चरम मानक नहीं हो सकते। यह सैनिक का कर्त्तव्य है कि जब उसे आह्वान प्राप्त हो तो वह युद्ध करे, यहाँ तक कि अपने बंधु-बांधवों पर भी गोली चलावे। परन्तु ऐसा या इससे मिलता-जुलता और कोई मानदण्ड मुक्त पुरुष पर लागू नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर, प्रेम या करुणा रखना, हमारी सत्ता के उच्चतम सत्य का अनुसरण करना और भगवान् के आदेश का पालन करना कोई कर्तव्य नहीं हैं। ये चीजें तो जब प्रकृति भगवान् की ओर ऊपर चढ़ती है वैसे-वैसे उसके धर्म हैं, एक आत्म-स्थिति से कर्म का प्रवाह है, आत्मा का उच्च सत्य है। कर्मों के मुक्त कर्ता का कर्म आत्मा से निःसृत इस प्रकार का प्रवाह ही होना चाहिये। यह भगवान् के साथ उसके आध्यात्मिक मिलन के स्वाभाविक परिणाम के रूप में उसे प्राप्त होना चाहिये अथवा उसके अन्दर प्रकट होना चाहिये, न कि मानसिक विचार एवं संकल्प और व्यावहारिक बुद्धि या सामाजिक भावना की किसी उन्नायक रचना से निर्मित होना चाहिये।
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।। १९।।
१९. इसलिये अनासक्त होकर सर्वदा किये जाने योग्य कर्म" को कर; क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य परम् पद को प्राप्त कर लेता है।
...तीन प्रकार के कर्म होते हैं; एक वह जो वैयक्तिक सुख-भोग के लिए यज्ञ के बिना किया जाता है, जो सर्वथा स्वार्थी और अहंकारपूर्ण होता है और जीवन के यथार्थ धर्म, ध्येय और उपयोगिता से वंचित रहता है, 'मोघं पार्थ स जीवति'; दूसरा वह कर्म जो होता तो है कामना से ही है पर यज्ञ के साथ, और इसका भोग केवल यज्ञ के फल के रूप में ही होता है, इसलिए उस हद तक यह कर्म समर्पित और पवित्रीकृत होता है; तीसरा वह कर्म जो किसी प्रकार की कोई कामना या आसक्ति से रहित होकर किया जाता है। यह अंतिम प्रकार का कर्म ही जीव को परम् पद प्राप्त कराता है, 'परमाप्नोति पूरुषः'।
इसमें श्रीअरविन्द अनासक्त कर्म, कर्तव्य कर्म की व्याख्या कर रहे हैं कि कर्तव्य कर्म क्या है। इसमें कर्त्तव्य कर्म की उच्चतर व्याख्या भी की गई है और निम्नतर भी। उच्चतर व्याख्या में तो व्यक्ति का किसी सामाजिक मानदण्ड से कोई लेना-देना नहीं होता। उसका अपना ही विधान होता है। विवेकानंद जी ने कहा कि जब व्यक्ति किसी कर्तव्य के रूप में कर्म करता है तो वह अपनी आत्मा के ऊपर साँकलें डालकर सारे जीवन भर तकलीफ पाता रहता है। परन्तु संसार में इस बात का बोध कैसे हो क्योंकि समाज में तो कर्तव्य का बहुत बड़ा अंकुश है, और सभी मनुष्यों को उसका हवाला दिया जाता है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन में केवल अपने सुख, आराम, पसंद, नापसंद आदि चीजों के अतिरिक्त और कुछ सोचते ही नहीं हैं। व्यक्ति अपने-आप से और कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है। उसे तो यह पता ही नहीं होता कि इन चीजों के अतिरिक्त जीवन में अन्य भी कोई प्रश्न हो सकता है। उसके जीवन का तो यही उद्देश्य होता है कि अच्छे मकान में रह गए, अच्छा खाना खा लिया, जो पसंद हों उन दोस्तों के साथ बैठ गए, जिससे मन प्रसन्न हो वह काम कर लिया, नौकरी में उन्नति मिल गई, आदि-आदि। इस प्रकार अधिकांश मनुष्य तो पशु सरीखा जीवन व्यतीत करते हैं। इस दायरे में लगभग निन्यानवे प्रतिशत मानवजाति आ जाती है। तो ऐसे में कर्तव्य बोध की तो परम आवश्यकता है। क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी होता है कि उसके लिए समाज का उस पर दबाव होता है, कर्तव्य का यह जुआ होता है कि उसे अपने बच्चों, माता-पिता, भाई-बहनों आदि का ध्यान रखना चाहिये। पश्चिम में तो कर्तव्य कर्म का अधिक दबाव नहीं रहा, वहाँ परिवार के प्रति कर्तव्य कर्म को समाप्त ही कर दिया गया है। कर्तव्य जैसी कोई चीज है ही नहीं। वहाँ कर्तव्य का बोध एक नागरिक के रूप में अपने देश के प्रति तो है, अन्य कोई नहीं।
परंतु इसकी उपयोगिता यही है कि यदि इसके अनुसार लोगों पर अंकुश न लगाया जाए तो वे घोर रूप से स्वार्थी ही रहेंगे। इसलिए वहाँ इस अंकुश का उपयोग है। परंतु जो व्यक्ति सन्मार्ग में चलना चाहता है उसके लिए कर्तव्य का कोई उपयोग नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो भीतर से यह बोध होना चाहिए कि उसे कौनसा कर्म करना चाहिये। यहाँ श्री अरविन्द कहते हैं कि यह कर्तव्य कर्म की अवधारणा यूरोपीय है अन्यथा जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तब सभी जीवों से प्रेम करना, भगवान् के प्रति निष्ठा रखना कोई कत्र्तव्य नहीं हैं। ये तो आध्यात्मिक जीवन के विधान हैं। जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो सहज रूप से ये उसके अंदर प्रकट होंगे ही। ऐसे में व्यक्ति किसी के साथ दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता। चेतना की ऐसी स्थिति में व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं रहती कि सबके साथ प्रेम रखना उसका कर्तव्य है। सभी के साथ प्रेम रखना तब उसका सहज स्वभाव हो जाता है और इससे भिन्न तो वह कर ही नहीं सकता। सामने आए किसी व्यक्ति के प्रति उसमें जो सद्भाव आ जाता है उसी के अनुसार वह कर्म कर देता है, क्योंकि यही उसका सहज स्वभाव होता है। ऐसी स्थिति में कर्त्तव्य के विचार की कोई उपयोगिता ही नहीं है। कर्तव्य बोध की उपयोगिता तो पाशविक मनुष्य के लिए है जिसे कि व्यवहार के लिए बाहरी नियम-विधान और अंकुश की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक पिपासु के लिए तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उसका तो एक ही ध्येय होता है कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कार्य उसके लिए आवश्यक है वह करे। उसके लिए कर्तव्यों के लबादे को ओढ़ने की कोई बाध्यता नहीं होती। और फिर सबका सच्चा सम्मान करना, सबके प्रति करुणा रखना, प्रेम करना, जीवमात्र के प्रति सहानुभूति रखना, इन्हें कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। ये सब तो उस प्रकृति के विधान हो जाते हैं जो परमात्मा की ओर चलती है। ये उसमें सहज रूप से आविर्भूत होंगे।
II. दिव्य कर्मों का सिद्धान्त
तो यह है गीता की यज्ञविषयक शिक्षा का अभिप्राय। इसका पूर्ण मर्म पुरुषोत्तम-तत्त्व के विचार पर निर्भर करता है, जिसका विवेचन अभी तक अच्छी तरह नहीं हुआ है गीता के अठारह अध्यायों में बहुत बाद में ही इस तत्त्व का स्पष्ट निरूपण हुआ है, और इसीलिए हमें गीता की प्रगतिशील वर्णन-शैली की मर्यादा का अतिक्रमण कर के भी इस केन्द्रीभूत शिक्षा की चर्चा पहले से ही करनी पड़ी। अभी श्रीगुरु... पुरुषोत्तम भाव की स्पष्ट भाषा में नहीं बोल रहे, अपितु 'मैं', कृष्ण, नारायण, अवतार-रूप से बोल रहे हैं उन्होंने पुरुषोत्तम की परम सत्ता का तथा अक्षर ब्रह्म के साथ - जिनमें ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर पूर्ण शान्ति और समता की अवस्था में अपने-आपको स्थिर करना पहला काम है और हमारी अति आवश्यक आध्यात्मिक माँग है उसका क्या संबंध है इसका एक संकेतमात्र दिया है, एक हल्की-सी झलक भर दिखायी है।... परन्तु यहाँ दो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। प्रथम यह कि इस प्रशान्त-स्थिर अक्षर आत्मा और प्रकृति के कर्म में एक विरोध प्रतीत होता है। जब हम इस अक्षर आत्मसत्ता में एक बार प्रवेश कर चुके तब फिर कर्म का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है और वह जारी कैसे रह सकता है.?... परमेश्वर यदि केवल यही अक्षर पुरुष हैं और व्यष्टि-पुरुष केवल कोई ऐसी चीज है जो उसमें से निकलकर उस शक्ति के साथ इस सृष्टि में आया है, तो जिस क्षण व्यष्टि-पुरुष लौटकर आत्मा में स्थित होगा उसी क्षण सारी सृष्टिक्रिया बन्द हो जाएगी और रह जाएगी केवल परम एकता और परम निस्तब्धता। दूसरी बात यह है कि यदि अब भी किसी रहस्यमय रूप से कर्म जारी रहे तो भी आत्मा जब सब पदार्थों के लिए सम है तब कर्म हों या न हों और हों तो चाहे जैसे भी हों, इसका कोई महत्त्व नहीं। ऐसी अवस्था में यह भीषण और विनाशकारी प्रकार का कर्म क्यों, यह रथ, यह युद्ध, यह योद्धा, यह दिव्य सारथी किसलिए?
गीता इसके उत्तर में परमेश्वर को इस रूप में प्रस्तुत करती है कि वे अक्षर पुरुष से भी महान् हैं, अधिक व्यापक हैं, जो एक ही साथ यह आत्मा भी हैं और प्रकृति में होनेवाले कर्म के अधीश्वर भी। परन्तु वे अक्षर ब्रह्म की सनातन अचलता, समता, कर्म और व्यष्टिभाव से अधिक श्रेष्ठता से प्रकृति के कर्मों का संचालन करते हैं। हम कह सकते हैं कि यही सत्ता की वह स्थिति है जिससे वे कर्मसंचालन करते हैं, और इस स्थिति में संवर्द्धित होने से हम उन्हीं की सत्ता और दिव्य कर्मों की स्थिति में संवर्द्धित हो रहे होते हैं।... इसलिए पुरुषोत्तम की धारणा, जो कि यहाँ अवतीर्ण नारायण, कृष्णरूप में दिखायी देते हैं, इसकी कुंजी है। इसके बिना निम्न प्रकृति से निवृत्त होकर ब्राह्मी स्थिति में चले जाने का परिणाम होगा मुक्त पुरुष का निष्क्रिय, और जगत् के कर्मों से उदासीन हो जाना; और इसके होने से यही निवृत्ति एक ऐसा उपाय हो जाती है जिससे जगत् के कर्मों को भगवान् के ही 'भाव, उन्हीं के स्वभाव, और उन्हीं की स्वतंत्रता के साथ लिया (किया) जाता है। शान्त ब्रह्म को अपने लक्ष्य के रूप में देखो तो संसार और उसके समस्त कर्मों का त्याग करना ही होगा; और उन ईश्वर, भगवान्, पुरुषोत्तम को अपने लक्ष्य के रूप में देखो, जो कर्म के परे होने पर भी कर्म के आंतरिक आध्यात्मिक कारण और ध्येय तथा मूल संकल्प हैं, तो संसार अपने सारे कर्मों के साथ जीत लिया जाता है और जगत् की दिव्य परात्परता में (अथवा उसका अतिक्रमण करते हुए) उसे अधिकृत कर लेता है। तब वह कारागार नहीं अपितु एक 'राज्यं समृद्ध' बन जाता है जिसे हमने निरंकुश अहंकार की सीमा का नाश कर, कामनारूपी जेलर के बंधन को काटकर और अपनी वैयक्तिक अधिकार-संपत्ति और भोग के कैदखाने को तोड़कर, आध्यात्मिक जीवन के लिये जीता है। तब मुक्त विश्वात्मभूत अंतरात्मा ही स्वराट्-सम्राट् हो जाती है।
xi.33
यदि एकमात्र वास्तविक चीज अक्षर पुरुष ही हो तो फिर कर्म करने का कोई उपयोग ही नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रहती। भगवान् श्रीकृष्ण, जो कि पुरुषोत्तम हैं, कह रहे हैं कि वे अक्षर पुरुष से श्रेष्ठ हैं इसीलिए दिव्य कर्म का अस्तित्व है। यदि ऐसा नहीं होता तो अर्जुन को सारी शिक्षा देकर वे युद्ध का आदेश कैसे कर सकते थे। उन लोगों की बुद्धि का यह दिवालियापन ही है जो कहते हैं कि गीता निष्काम कर्म करके सब कुछ छोड़ देने की, संसार को त्याग देने की शिक्षा देती है। भला गीता ऐसा कैसे कह सकती है क्योंकि अर्जुन को तो उसे घोर युद्ध कर्म में नियोजित करना है, और संसार को मिथ्या-माया बताकर तो ऐसा किया नहीं जा सकता। इसलिए पुरुषोत्तम की बात ही गीता का सार है और फिर उन्हें समर्पित करके जो कर्म किए जाते हैं वे दिव्य कर्म होते हैं। आजकल की आधुनिक धार्मिक शिक्षा के अनुसार निष्काम कर्म ही दिव्य कर्म हैं। अब गीता इन विषयों से निकलकर अधिक जटिल और साधना के अधिक गहन विषयों में प्रवेश करती जाएगी, अधिक गहरी होती जाएगी।
यहाँ गीता में वर्णित कुछ बातें मानसिक हैं तथा कुछ महसूस करने की हैं। मानसिक बात तो सरल है। गीता आरम्भ में केवल दो स्थितियों की बात करती है। एक स्थिति में तो पुरुष प्रकृति के चंगुल में है, उसकी कैद में है। ठीक-ठीक किस प्रकार की कैद में है वह तो हर पुरुष की स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न है। पर इसमें सर्वसामान्य कैद है जड़ प्रकृति के, मानसिकता के, भावना आदि के विभिन्न नियम जिनके अधीन रहकर वह जो कुछ भी उसे मिल जाता है उतना भर ले लेता है अन्यथा उस कैद में तकलीफ पाता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर निरंतर अपनी कामनाओं, इच्छाओं, लोभ लालच से कुछ प्राप्त करके सुख पाने का प्रयत्न करता रहता है। परन्तु वह यह नहीं समझता कि इन प्रकृति के नियमों में कोई सार नहीं है और इनसे उसे कभी कुछ नहीं मिल सकता। और इनके अंतर्गत रहते हुए जो भी निम्न सुख-भोग उसे प्राप्त हो रहा है वह भी अंततः उसे नहीं प्राप्त होने वाला और उनका नाश होने वाला है। इस प्रकार मनुष्य अपना सच्चा स्व खो बैठता है और जीवन भर सारी चीजों में यह व्यवस्था करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार थोड़ा-सा आराम मिल जाए, थोड़े से साधन हों तो उत्तनी चिन्ता न रहे जिससे कि यदि काम न भी करना पड़े तो भूखे न मरे, मकान हो जाए तो रहने का साधन हो जाये, कुछ इस तरह के मित्र हों, जानकार हों कि कभी उसे किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यही अधिकांशतः कम या अधिक हम सबकी स्थिति होती है और इसमें रहने वाला व्यक्ति इन्हीं चीजों को पाने का प्रयत्न करता रहता है। इसे कहते हैं क्षर पुरुष, अर्थात् वह जो नष्ट होने वाला है। इस प्रकार के जीवन में कोई सार नहीं है। मनुष्य प्रकृति के सत्त्व, रज, तम में फंसा रहता है और द्वन्द्व - सफलता-असफलता, सुख-दुःख, हानि-लाभ, शीत-उष्ण- आदि चलते रहते हैं और इनमें मनुष्य कीड़े की तरह बिलबिलाता रहता है।
गीता आरम्भ में ही कहती है कि यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के अन्दर प्रभु का एक ऐसा रूप है जो इस प्रकृति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, वह शांत है, सर्वत्र व्याप्त है, प्रकृति की किसी भी क्रिया से विचलित नहीं होता। उसका अपना जो आनन्द है, जो सुख है, जो समता है वह अक्षुण्ण है, संसार में चाहे कुछ भी हो जाए परन्तु प्रकृति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अतः मनुष्य को सर्वप्रथम साक्षी होकर उस स्थिति में जाना होगा। और साक्षी रूप से प्रकृति के सारे क्रिया-कलापों का अवलोकन करना होगा तब व्यक्ति समझेगा कि यह सब क्या हो रहा है। आरम्भ में गीता इस स्तर तक आरोहण करने के लिए सांख्य शास्त्र का वर्णन करती है, जिसमें व्यक्ति को आत्म-विवेचन द्वारा, ज्ञान द्वारा इसके विविध सोपानों पर आरोहण करते हुए साक्षी भाव तक उठने का प्रयास करना होता है। जैसा कि रमण महर्षि ने बताया कि हमें आत्म-विवेचन द्वारा यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि 'मैं कौन हूँ"? 'मैं इन्द्रियाँ नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, तब फिर 'मैं कौन हूँ। यह एक स्थिति है। जैसे ही व्यक्ति इस स्थिति से तादात्म्य स्थापित कर लेता है वैसे ही वह प्रकृति के क्रियाकलापों से ऊपर उठ जाता है और उसे जीवन में समझ में आने लगता है कि व्यर्थ ही वह अभी तक विचलित हो रहा था। तो यह एक अक्षर ब्रह्म में स्थिति की अवस्था है। गीता अभी तक इससे आगे नहीं गई है। इसीलिए श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि फिर दिव्य कर्मों के संपादन की समस्या का हल क्या होगा? दिव्य कर्म होंगे ही कैसे? क्योंकि क्षर की स्थिति में तो मूर्खता के कर्म ही होंगे जिसमें व्यक्ति केवल सुख की ही लालसा करता रहता है और सुख-भोगों की परछाइयों का पीछा करता रहता है।
इसके समाधान के रूप में कुछ लोगों ने दूसरी स्थिति अक्षर पुरुष में अकर्म की बताई है। जहाँ पूर्ण शांति है, प्रशांति है, समता है। कर्म होने या नहीं होने से कोई सरोकार नहीं होता। इस स्थिति में आकर कर्म को लिप्सा और जिस उद्देश्य से कर्म किए जाते हैं वह सारा आधार ही समाप्त हो जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। परंतु इस स्थिति में तो कर्म की कोई संभावना नहीं है। इस स्थिति में रहकर व्यक्ति कर्म क्यों करेगा, कर्म करने का हेतु ही क्या होगा? अतः, क्षर पुरुष की स्थिति में तो अज्ञानपूर्वक कर्म किए जाते हैं और दूसरी अक्षर की स्थिति में, जहाँ शांति है, प्रशांति है, वहाँ संस्कारवश या इन्द्रियों के कर्म करने के अभ्यास के कारण यदि कर्म जारी रहते हैं तो भी व्यक्ति उनको निर्लिप्त भाव से वैसे ही देखता रहता है जैसे अपने से भिन्न दूसरे लोगों को देखता है और ऐसे में यह मनोभाव रहता है कि जब भी शरीर छूट जाये तब उसके परे चले जाओ। यह बुद्धिमार्गियों का, शंकराचार्य आदि ज्ञानमार्गियों का, सांख्य-शास्त्र का एक पारम्परिक समाधान है। इसके अतिरिक्त, वेदवाद कहता है कि अमुक कर्म करने से अमुक फल की प्राप्ति होगी। इन्हीं सब दृष्टिकोणों के कारण ही श्रीअरविन्द कहते हैं कि ऐसे में तो फिर दिव्य कर्म की तो कोई संभावना ही नहीं है, और ऐसे में जिस प्रकार के भयंकर कर्म का गीता आदेश कर रही है उसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता।
इसलिए, वे कहते हैं कि दिव्य कर्म का समाधान होता है नारायण के भाव में। श्रीकृष्ण शुरू में क्षर और अक्षर पुरुष की चर्चा करते हैं परन्तु उसके बाद में 'मैं', 'अहं', 'माम्', कहकर गीता का रहस्य बताते हैं। यही है वह रहस्य जो केवल गीता का ही नहीं अपितु हमारे सारे जीवन का भी रहस्य है। और वह है भगवान् का स्वयं का व्यक्तित्व, उनका सत्स्वरूप जिसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। केवल वे ही अकेले विद्यमान हैं और कोई नहीं है। बाकी सारे उन्हीं के रूप हैं। यदि व्यक्ति एक बार उनकी झलक पा ले तो फिर सब कुछ उसके और उनके बीच का खेल और लीला बन जाता है। तब ऐसा छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा कोई कर्म नहीं रह जाता जो उनके द्वारा समर्थित नहीं हो, उनके द्वारा न किया जाता हो। इस प्रकार कर्मों का जो दुःखमय स्वरूप है, जो अच्छा-बुरा स्वरूप है वह समाप्त हो जाता है। फिर तो सब केवल दिव्य लीला बन जाती है। व्यक्ति और भगवान् के बीच प्रेम का आदान-प्रदान बन जाता है और इसी के लिए तो उन्होंने सृष्टि की है। यह सृष्टि वह शाश्वत वृंदावन है जिसमें शाश्वत बालक शाश्वत लीला कर रहा है। यह उसका वृंदावन है और इसमें उसकी लीला चल रही है। इस परिदृश्य में तो सब रूप ही बदल जाता है और ऐसे में कर्म-अकर्म आदि सब विचारणाएँ ही बदल जाती हैं। यदि इस खेल में कोई वृत्रासुर या कोई अघासुर आ जाता है तो उसे तो वे क्रीड़ा के भाव में ही नष्ट कर देते हैं। वैसे ही यह कुरुक्षेत्र भी एक प्रसंग स्वरूप सामने आ गया है और भगवान् कहते हैं कि 'निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्', तू तो बस निमित्त बन कर इन्हें नष्ट कर दे। ज्यों ही व्यक्ति परमात्मा के उस अस्तित्व की, उस व्यक्तित्व की, जो कि उसके जीवन का सार है, एक बार जरा सी झलक भी पा लेता है तो सम्पूर्ण सत्ता में रसक्रिया होनी आरंभ हो जाती है और तभी सच्चे कर्म का रहस्य पता चलता है अन्यथा तो कर्म एक रोग समान है। वास्तव में किन्हीं निम्न हेतुओं की प्राप्ति के लिए, किसी कामना की पूर्ति के लिए संसार में कर्म करने से अधम तो कुछ है ही नहीं। पर यदि क्रीड़ा या लीला के भाव से कर रहा हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो यह है गीता के पुरुषोत्तम का रहस्य जो क्षर और अक्षर दोनों से बहुत महान् हैं। और ये दोनों तो उनकी दो स्थितियाँ मात्र हैं जिनसे वे स्वयं परे हैं।
xi.33
वास्तव में तो केवल वे ही अस्तित्वमान हैं, बाकी तो प्रतीतियाँ मात्र हैं। और यह सब भी आखिर बुद्धि का एक जंजाल ही है, अन्यथा वास्तव में तो न क्षर है और न अक्षर। पुरुषोत्तम के अतिरिक्त यहाँ और कुछ है ही नहीं। यह सब तो उनकी क्रीड़ा मात्र है। गीता की शिक्षा को व्यक्ति सच्चे रूप में तभी समझ सकता है जब उसे परमात्मा की झलक मिल जाए और वह उनकी चेतना में प्रवेश कर जाए। यह बड़ी विलक्षण चीज है। वास्तव में उन्हीं का खेल है, उन्हीं का वृंदावन है, उन्हीं की प्रकृति है, उन्हीं का सब कुछ है और वे ही क्रीड़ा कर रहे हैं। इस चेतना में तो सारे कर्म दिव्य हैं, जिनमें बड़ा आनन्द है। तभी तो भगवान् स्वयं कहते हैं कि मुझे त्रिलोकी में किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी मैं कर्म करता हूँ। ये सब बातें 'दिव्य कर्म के सिद्धान्त' में आने वाली हैं।
भगवान् द्वारा स्वयं का उदाहरण दिये जाना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कर्म क्या है? भगवान् का खेल है, आनन्द नृत्य चल रहा है। यदि व्यक्ति जरा-सा भी उनके साथ सम्पर्क में आ जाए तो उसके सारे जीवन का सारा समीकरण बिल्कुल बदल जाता है। अब तो वे श्रीमाँ-श्रीअरविन्द के रूप में यहाँ आ चुके हैं। पुरुषोत्तम ने स्वयं को दो शरीरों में हमारे सामने प्रकट किया है जिनसे हम सम्पर्क कर सकते हैं, सम्पर्क होता है, कर लेते हैं, तब फिर व्यक्ति को अधिक-से-अधिक और घोर से घोर कर्म करने में भी कोई संकोच नहीं हो सकता। क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई तो है ही नहीं। सर्वत्र वे स्वयं ही तो विद्यमान हैं और दूसरे उन्हीं के रूप हैं और वे परस्पर खेल कर रहे हैं। गीता का रहस्य तो यही है। 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज', वे आत्मा को कहते हैं कि इन सबको छोड़ कर मेरी शरण में आ जा। ये ब्रह्म, ईश्वर आदि सब भ्रम हैं। श्रीकृष्ण पहले तो अर्जुन को कहते हैं कि 'तू उसकी शरण ले जो सम्पूर्ण सृष्टि को चलाता है' परंतु बाद में उससे कहते हैं कि सब छोड़ कर मेरी शरण में आ जा। 'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः' मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, चिंता ही मत कर।
iii.62
श्रीअरविन्द के अनुसार संपूर्ण गीता केवल उन दो श्लोकों को बताने के लिए, आत्मा को अपनी प्राकृत स्थिति से उठा कर इस स्थिति तक ले आने के लिए तैयारी मात्र है। भगवान् ने एक गुरु के रूप में उपदेश आरंभ किया जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण आया हूँ, मुझे समझाइये, और अंत में एक प्रेमी के रूप में उन्होंने अपनी बात का समापन कर दिया। यहाँ सच्चा व्यवहार तो प्रेम का ही है। प्रेम के अतिरिक्त और है ही क्या। साधना, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग सब बताकर अन्त में भगवान् कहते हैं कि मेरी शरण में आ। इसके बाद पुरुषोत्तम की क्रिया आरम्भ होती है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में यह अभीप्सा जगा सके, यह विचार जगा सके कि उसे केवल भगवान् की ओर ही जाना है तो मानो कि उसका सब कुछ हो चुका अन्यथा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अन्यथा जीवन एक दुःखद विडम्बना है। बिना प्रभु के स्पर्श के जीवन एकदम बेकार है।
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ।। २० ।।
२०. कर्म के ही द्वारा जनक आदि पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोकसंग्रह को दृष्टि में रखते हुए भी तुझे कर्म ही करना चाहिये।
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।। २१।।
२१. श्रेष्ठ मनुष्य जैसा-जैसा आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं; वह (श्रेष्ठ मनुष्य) जिस आदर्श या मानक को रचता है दूसरे साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं।
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ।। २२।।
२२. हे पार्थ! तीनों लोकों (भौतिक, प्राणिक, मानसिक) में मेरे लिये कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसके करने की मुझे आवश्यकता हो, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो और जिसे प्राप्त करना शेष हो, किंतु फिर भी मैं कर्म के मागों में ही रत रहता हूँ।
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।
मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।। २३ ।।
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ।। २४।।
२३-२४. क्योंकि हे पृथापुत्र अर्जुन ! मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिये जो मैं कभी आलस्यरहित होकर कर्मों के मार्ग में न रहूँ, यदि मैं कर्म न करूँ तो ये मनुष्य नष्ट हो जाएँ और मैं संभ्रम का स्रष्टा और इन जीवों की हत्या करनेवाला (विनाश करनेवाला) होऊँगा।
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ।। २५।।
२५. हे भारत! अज्ञानी मनुष्य कर्म में आसक्त होकर जिस प्रकार कर्म करते हैं, ज्ञानी मनुष्य को अनासक्त होकर लोकसंग्रह को लक्ष्य में रखते हुए उसी प्रकार कर्म करने चाहिये।
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ।। २६।।
२६. ज्ञानी मनुष्य को चाहिये कि वह अपने कर्मों में आसक्ति रखनेवाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भेद न उत्पन्न करे; योगयुक्त रहते हुए और ज्ञानपूर्वक संसार के लिये आवश्यक समस्त कमाँ को स्वयं करते हुए उन्हें उन कर्मों में प्रवृत्त करे।
इन सात अद्भुत श्लोकों से अधिक महत्त्वपूर्ण श्लोक गीता में कुछ हो और हैं।
परन्तु हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि इन श्लोकों का आधुनिक व्यवहारवादी वृत्तिवालों की तरह अर्थ लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो किसी उच्च और दूरस्थ आध्यात्मिक संभावना की अपेक्षा जगत् की वर्तमान अवस्था से ही मतलब रखते हैं, और इन श्लोकों का उपयोग समाज-सेवा, देश-सेवा, जगत्-सेवा, मानव-सेवा तथा आधुनिक बुद्धि को आकर्षित करनेवाली सैकड़ों प्रकार की समाज-सुधार की योजनाओं और स्वप्नों का दार्शनिक और धार्मिक समर्थन करने में करते हैं। यहाँ इन श्लोकों में जिस विधान की घोषणा की गयी है वह किसी व्यापक नैतिक और बौद्धिक परोपकारिता का नियम नहीं, अपितु ईश्वर के साथ और जो ईश्वर में रहते तथा जिनमें ईश्वर रहता है उन प्राणियों के इस जगत् के साथ आध्यात्मिक एकता का विधान है। यह विधान व्यक्ति को समाज और मानव-जाति के अधीन बना देने या मानव-समष्टि की वेदी पर व्यक्ति के अहंकार की बलि देने का आदेश नहीं है, अपितु व्यक्ति को ईश्वर में परिपूर्ण करने और अहंकार को सर्वालिंगनकारी भगवत्ता की एकमात्र सच्ची वेदी पर बलि चढ़ाने की आज्ञा है। गीता विचारों और अनुभूतियों की एक ऐसी भूमिका पर विचरण करती है जो आधुनिक मन के विचारों और अनुभूतियों की भूमिका से ऊँची है। आधुनिक मन वस्तुतः अभी अहंकार की कुंडलियों को काटने के लिए संघर्ष करने की अवस्था में है; परन्तु अब भी अपनी दृष्टि में संसारबद्ध है और अपनी मनोवृत्ति में आध्यात्मिक की अपेक्षा बौद्धिक और नैतिक है। देश-प्रेम, विश्वबंधुत्व, समाज-सेवा, समष्टि-सेवा, मानव-सेवा, मानव-जाति का आदर्श या धर्म, ये सब व्यष्टिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय अहंकाररूपी पहली अवस्था से निकलकर दूसरी अवस्था में जाने के लिए सराहनीय साधन हैं, इस अवस्था में पहुँचकर व्यक्ति, जहाँ तक कि बौद्धिक, नैतिक और भावावेगमय स्तर पर संभव है, यह अनुभव करता है कि उसका अस्तित्व दूसरे सब प्राणियों के अस्तित्व के साथ एक है- यद्यपि उस स्तर पर ऐसा अनुभव वह सर्वथा उचित रूप से और पूर्ण तरीके से, अपनी सत्ता के पूर्ण सत्य के अनुसार प्राप्त नहीं कर सकता। परन्तु गीता का चिंतन इस दूसरी अवस्था के भी परे जाकर हमारी विकसनशील आत्म-चेतना की एक तीसरी अवस्था में पहुँच जाता है जिसमें पहुँचने के लिये दूसरी अवस्था केवल आंशिक प्रगति है।... गीता द्वारा यहाँ दिया विधान मानवश्रेष्ठ, अतिमानव, आध्यात्मिकृत मनुष्य या सर्वश्रेष्ठ का विधान है, परंतु यह कोई नीत्शे के अर्थ में एक एकांगी तथा बेढंगे अतिमानव का विधान नहीं है, कोई यूनानी ओलिम्पस, अपोलो या डायोनीसियस जैसी अथवा देवदूत और दैत्य के जैसी अतिमानवता का विधान नहीं है, अपितु गीता का अतिमानव वह मनुष्य है जिसका सारा व्यक्तित्व एकमेव परात्पर और विश्वव्यापी भगवान् की सत्ता, प्रकृति और चेतना के प्रति उत्सर्ग हो गया है और जिसने अपने क्षुद्र स्वत्व को खोकर अपने महत्तर आत्मतत्त्व को पा लिया है, जो दिव्यीकृत हो चुका है।
-----------------
*...हमारी मानसिक चेतना का विस्तार कर के अहंकारमय द्वंद्वों के अनुभव से बाहर निकलकर समग्र चेतना के साथ एक अनियमित एकता साधित करने से सहज ही जगत् की सापेक्षताओं की सुप्रतिष्ठित व्यवस्था में व्यवस्थित मानवजाति के सक्रिय जीवन में असमर्थता और संभ्रम (बुद्धिभेद) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गीता में जो ज्ञानी मनुष्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अज्ञानी मनुष्य के जीवन के आधार और विचार के आधार को विचलित न करे, उसका यही मूल कारण है। क्योंकि उसके उदाहरण से प्रेरित होकर किन्तु उसके कर्म के सिद्धांत या आधार को समझने में असमर्थ होने के कारण, वे किसी उच्चतर आधार को प्राप्त न कर के स्वयं अपने (जीवन और कर्म के) मूल्यों की व्यवस्था को भी खो बैठेंगे।
बंकिमचन्द्र सरीखे आजकल के बहुत से टीकाकारों ने गीता पर जो टीकाएँ की हैं कि और इस पर बल दिया है कि 'कर्तव्यं कर्म करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, सबका भला करो, मनुष्यजाति का भला करो, दुःख-दर्द मिटाओ, अस्पताल खोलो, स्कूल खोलो, शिक्षा दो', आदि-आदि, परंतु गीता ऐसी सांसारिक शिक्षाओं के स्तर पर व्यवहार नहीं करती। गीता में ऐसी बातें नहीं हैं। गीता एक सर्वथा भिन्न और अति उच्च स्तर पर व्यवहार करती है। हम जिस स्तर पर हैं, जितनी हमारी समझ है हम केवल उतना ही समझ सकते हैं। हमारे स्तर के अनुसार हमारे भिन्न-भिन्न स्तर के दृष्टिकोण होते हैं। पहला यह है जियमें मनुष्य इस धरती पर केवल अपने अहं के जीवन में, सुख, सम्पत्ति, परिवार, बड़ाई आदि हजार तरीके की चीजों में कीड़े की तरह बिलबिलाते रहते हैं। इससे ऊपर का दृष्टिकोण यह है जब व्यक्ति कहता है कि 'हम लोग तो सब एक ही हैं, सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, सारा राष्ट्र भी परमात्मा का ही स्वरूप है, सारी मनुष्यजाति एक है इसलिए मनुष्यजाति की सेवा करो, देश की सेवा करो, देश को ऊपर उठाओ, सबकी भलाई करो, इस तरह से करो कि मनुष्य सब अपने गन्तव्य स्थान में अच्छे कर्म कर के जाएँ, इससे आगे आज का सांसारिक विचार जा ही नहीं सकता। परंतु गीता इस स्तर पर व्यवहार नहीं करती। गीता की दृष्टि केवल परम प्रभु, पुरुषोत्तम पर है। यहाँ जिन कर्मों की चर्चा हो रही है वह तो उन्हीं की प्रसन्नता के निमित्त दिव्य कर्मों की बात है। उन कर्मों का इन कमों के साथ कोई अधिक संबंध नहीं है। हर जगह, हर चीज में केवल पुरुषोत्तम ही हैं, उन्हीं के साथ हमारा खेल है। इस दृष्टिकोण से जब हम कर्म करेंगे तो सारा मापदण्ड, कर्म का स्तर, भावना, सही-गलत का निर्णय बिल्कुल भिन्न तरह का होगा। परन्तु जब व्यक्ति अपने अहं पर केन्द्रित होकर सबकी भलाई करने के लिए कहता है तो वह केवल अपने अहं के लिए ही सोचता है। यदि हम कहते हैं कि 'मेरा देश' तो यह भाव भी इसलिये होता है क्योंकि यह 'मेरा' देश है, या फिर मनुष्य-जाति के लिए भाव हो तो वह भी इसलिये क्योंकि 'मैं' मनुष्य हूँ। इस दृष्टिकोण में हम निचले से बस कुछ थोड़े से विशालतर अहं की सेवा ही कर रहे होते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। परन्तु 'सर्वत्र पुरुषोत्तम की लीला ही है' इस दृष्टिकोण में तो अहं रहता ही नहीं है। इस भाव में तो केवल एक 'वे' ही हैं जो हमारा सच्चा सार-तत्त्व होते हैं। फिर 'वे' हमें मानसिकता के, मनुष्य के स्तर के बहुत परे ले जाते हैं। तब हम प्रकृति के दास नहीं रह जाते। वहाँ प्रकृति के नियम-विधान लागू नहीं होते। प्रकृति के नियम तो केवल ऐसे अभ्यास मात्र हैं जो प्रकृति उनकी सेवा के लिए, उनके कार्य के लिए बनाती है। प्रकृति जो कुछ भी करती है केवल 'उनकी' प्रसन्नता के निमित्त ही करती है।
गीता पुरातन संस्कृति की पाँच हजार वर्ष पुरानी पुस्तक है। इसमें जो संदेश है वह यह है कि भगवान् को कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी वे कर्म में रत रहते हैं। यह एक बड़ी विलक्षण और महत्त्वपूर्ण बात है कि यहाँ सब कुछ उनका आनन्द-नृत्य है। किसी प्रकार के फल के लिए वे कर्म नहीं करते। प्रकृति तो उनके अधीन है। यह सब तो प्रभु का खेल मात्र है और इस खेल में हमें भाग लेना है। ज्यों ही अहं खत्म हुआ तो हम उस चेतना में चले जाते हैं जिसमें उनके सम्पर्क मात्र से सारा जीवन ही बदल जाता है। गीता हमें उसी की ओर ले जा रही है। अर्जुन की आत्मा को तैयार कर रही है कि उसके भाव जगे और वह पूछे कि 'प्रभु आप कौन हैं, मुझे अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन कराएँ।' परन्तु उस रूप को देखने के बाद वह भ्रमित हो जाता है और बहुत सारे नए प्रश्न उसके मन में आते हैं। उसे सब समझाने के बाद अन्त में भगवान् कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग कर के बस केवल मेरी शरण ग्रहण कर।
यही गीता की मूल बात है, बाकी सब तो सहायक कहानी मात्र ही है। स्वयं भगवान् के मुख से यह प्रस्फुटित हुई है, पुरुषोत्तम स्वयं बोल रहे हैं। मनुष्य जब दिग्भ्रमित हो, उसके मन में जो विकार आते हैं, उसके मन और प्राण में जो पहेलियाँ आती हैं उन सबका भगवान् ने मनुष्य के स्तर पर ही समाधान किया और फिर अर्जुन को समझाया कि तू इन सबकी चिंता मत कर और केवल मेरी शरण में आ। इस प्रकार यह दिव्य कर्म का सिद्धांत पुरुषोत्तम के दर्शन पर आधारित है।
ⅲ23
यहाँ एक श्लोक और आता है जिसके बारे में श्रीअरविन्द कहते हैं कि यह ही हमारे जीवन का सार है। वह है - 'मम् वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः'। 'सब मनुष्य सब तरीके से मेरे ही रास्ते पर चलते हैं। आखिर इसके अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है? संसर में और कुछ है ही नहीं। मनुष्य को केवल उन्हीं के रास्ते पर चलना होगा। और उनकी लीला को समझने के लिए व्यक्ति को उनकी चेतना में जाना होगा। यदि हम जादूगर की लीला को समझना चाहते हैं तो हमें जादूगर के मस्तिष्क में प्रवेश करना होगा। जीवन का यह सबसे बड़ा रहस्य है। सभी कोई हर तरीके से, चाहे किसी भी रास्ते से क्यों न जा रहे हों किन्तु सब जा उसी की ओर रहे हैं, अन्य कोई गन्तव्य स्थान किसी भी मनुष्य का नहीं है।
गीता निश्चयात्मक रूप से कहती है कि मुक्त मनुष्य का कर्म कामना से परिचालित नहीं होना चाहिये, अपितु लोक के संग्रह, उसके शासन, मार्गदर्शन तथा प्रचालन तथा इसे इसके नियत पथ पर बनाए रखने की दिशा में होना चाहिए। इस उपदेश का यह अर्थ किया गया है कि क्योंकि संसार एक ऐसा भ्रम अथवा माया है जिसमें अधिकतर मनुष्यों को रखना ही होता है - चूंकि वे मुक्ति के अयोग्य होते 3 -3 hat H बाहरी रूप से इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि वह सामाजिक नियम द्वारा उनके लिये निर्दिष्ट आचारिक कर्मों में उनकी आसक्ति को दृढ़ बनाये रखे। यदि ऐसा ही हो तो यह एक हीन और तुच्छ नियम होगा और प्रत्येक उदात्त-हृदय व्यक्ति इसका त्याग कर अमिताभ बुद्ध के दिव्य व्रत, भागवत' की उत्कृष्ट प्रार्थना और विवेकानन्द' की उत्कट अभीप्सा का ही अनुसरण करना चाहेगा।
परंतु, यदि हम इस भाव को स्वीकार करें कि यह संसार प्रकृति की एक दिव्य रूप से परिचालित गति है, जो मनुष्य के अन्दर उत्पन्न होकर ईश्वर की ओर ईश्वरोन्मुख गति करती है और इसी कार्य में, गीता के ईश्वर कहते हैं कि वे निरन्तर रत हैं, चाहे स्वयं उनके लिये ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जो उन्हें अभी प्राप्त करनी हो, - तो इस महान् उपदेश का गंभीर और सत्य आशय हमारे सामने प्रकट हो जायेगा। उस दिव्य कर्म में भाग लेना और संसार में ईश्वर के लिये जोना ही कर्मयोगी का विधान होगा; और संसार में ईश्वर के लिये जीना और इसलिए इस प्रकार कर्म करना कि भगवान् अपने-आप को अधिकाधिक प्रकट कर सकें और संसार अपनी अज्ञात यात्रा के चाहे जिस भी मार्ग से हो, आगे बढ़ता हुआ दिव्य आदर्श के अधिक निकट पहुँच सके।
गीता के संदेश को तीन दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। पहला तो यह कि जैसा लोग कहते हैं और स्वयं भगवान् ने भी कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। चूँकि संसार इसी तरीके का है कि यदि लोगों को यह बात नहीं बताई जाए तो वे निष्कर्मण्य हो जायेंगे। इसलिए उन मूढ़ जनों को कहो कि शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। इस तरह उनको कर्म में लगाये रखो जिससे वे बोझा ढोते रहें और भगवान् का संसार चलता रहे। और जिस व्यक्ति की आत्मा पवित्र है, जिसने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है और जो वास्तव में इस योग्य है वह भगवान् की ओर बढ़ कर इससे निकल जायेगा, बाकी सब इस साँचे में पिसते रहेंगे।
परन्तु श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि यह तो बहुत तुच्छ बात है। इससे श्रेष्ठ तो दूसरा दृष्टिकोण अमिताभ बुद्ध का है जो कहते हैं कि 'जब तक एक भी आत्मा ऐसी है जो कष्ट में है तब तक मैं निर्वाण में नहीं जाना चाहूँगा। मैं उसकी सहायता करूंगा, उसकी प्रतीक्षा करूंगा।' भागवत् के अनुसार 'मुझे न तो अष्ट सिद्धि चाहिए, न निर्वाण चाहिए, न मुक्ति चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि सारे जीवों की सेवा करूँ, उनका दुःख मैं स्वयं सहन करता रहूँ और उनको आगे बढ़ाऊँ।' या फिर विवेकानन्द जी जैसा कहते हैं वह भी हमने पढ़ ही लिया है। पहले दृष्टिकोण से तो यह दूसरा दृष्टिकोण – अमिताभ की प्रार्थना, भागवत् के और विवेकानन्द जी के उद्गार - ही श्रेष्ठ है। परन्तु गीता का संदेश इन किन्हीं भी दृष्टिकोणों से सीमित नहीं होता।
-------------------
* अमिताभ बुद्ध... जब उनकी आत्मा निर्वाण की ड्योढ़ी पर पहुँची तो वे वापस मुड़े और प्रतिज्ञा की कि जब तक एक भी जीव दुःख और अज्ञान में रहेगा तब तक वे इसे कभी नहीं लाँधेंगे।
* "मुझे न तो आठों सिद्धियों से युक्त परम पद की कामना है और न पुनर्जन्म से छुटकारे को। मैं चाहता हूँ कि सभी संतप्त प्राणियों का दुःख अपने ऊपर ले लूँ और उनके अन्दर प्रविष्ट हो जाऊँ जिससे वे कष्ट से मुक्त हो जायें।"
* उस महान् वेदान्ती ने लिखा "मुझे अपनी मुक्ति की कोई इच्छा नहीं रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं फिर-फिर पैदा होऊँ और हजारों कष्ट भोगूँ जिससे मैं उस एकमात्र ईश्वर को पूजा कर सकूँ जो वस्तुतः सत् है: उस एकमात्र ईश्वर की जिसे मैं मानता हूँ, जो सब आत्माओं का अंतिम परिणाम अथवा कुल योग है, और इससे भी बढ़कर वह ईश्वर जो सब जातियों और उपजातियों के दुष्ट जनों में है, मेरा वह ईश्वर जो सब दीन-दुःखियों में है, वह दरिद्रनारायण ही मेरा विशेष पूजापात्र है। जो उच्च और नीच, सन्त और पापी, देवता और कृमि है, उसकी पूजा करो, दृश्य, ज्ञेय, वास्तविक और सर्वव्यापक की पूजा करो; अन्य सभी मूर्तियाँ तोड़ फेंको।"
गीता लोकसंग्रह की बात करती है। लोकसंग्रह क्या है? यह तो प्रभु की लीला है। ऐसी लीला है जिसमें प्रभु अपनी अन्तरंग चीजें, अपनी अन्तर की बातें, अपने सत्य, अपना प्रेम उजागर कर सबके सामने ला रहे हैं और अधिकाधिक रूप से ला रहे हैं। इसमें बड़ा भारी आनन्द है। उनको प्रकट करने के लिए इस तरह की चीजें, इस तरह के साँचों की आवश्यकता है जिन्हें हमारी बुद्धि समझ नहीं सकती। प्रभु को प्रकट करने की जो लीला चल रही है ये सब उनके वर्धित होते दृश्य हैं, इसमें जैसे नाटक की सब चीजों को, सामान को, पर्दों को ठीक रखा जाता है जिससे कि अन्य दृश्य बखूबी सामने आ सकें, उसी प्रकार इस तरीके के काम लोकसंग्रह हैं जिनमें व्यक्ति यदि लगा रहता है तो प्रभु की लीला के और अधिक अंतरंग दृश्य प्रकट होते हैं। हम उनके और अधिक निकट आ सकते हैं और स्वयं को जान सकते हैं। उन सत्यों को प्रकट कर सकते हैं जो आज तक कभी किसी ने प्रकट नहीं किए। इसलिए मनुष्य कर्म करता है। वहाँ कोई कामना पूर्ति का प्रश्न नहीं है, वह तो आनन्द के लिए करता है क्योंकि वह तो स्वयं प्रभु का रूप है, उनका सखा है, उनका प्रेमी है। उनकी लीला में उनको प्रकट करने में प्राप्त होने वाले आनन्द के लिये वह कर्म करता है। यही कर्मयोगी के कर्म का उद्देश्य हो सकता है, अन्य कोई उद्देश्य उसके लिये नहीं रहता।
पहले दो दृष्टिकोण तो मनुष्य पर केन्द्रित हैं जबकि यह तीसरा दृष्टिकोण पुरुषोत्तम पर केन्द्रित है। गीता का जो संदेश है वह पुरुषोत्तम पर केन्द्रित है। पहले दृष्टिकोण के अनुसार माया का काम चलता रहेगा और जो उसमें से बच सके, वह बच कर निकल जाये। दूसरे दृष्टिकोण में अन्य लोगों, देश अथवा समाज की भलाई करने की बात है। तीसरा दृष्टिकोण है प्रभु के आनन्द का। इसमें किसी प्रकार की कोई भलाई करने जैसी कोई बात नहीं है अपितु दिव्य विधान में जो आवश्यक है वही करने की बात है। अर्जुन को तो भगवान् किसी भलाई के काम में नहीं लगा रहे, उसे तो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में अमिताभ बुद्ध की बात कहाँ लागू होती है? परंतु क्योंकि लोकसंग्रह के अंदर इतनी ये बाधाएँ आ खड़ी हुई हैं इसलिए यह संहारकर्म आवश्यक है। यह तो वैसा ही है जैसे मानो पिछले दृश्य में बहुत अधिक सामान मंच पर आ गया था, इसलिये अब दूसरे दृश्य के लिए मंच को साफ करना आवश्यक है ताकि मुरली बजाई जा सके और गोपियों का नृत्य हो सके। यहाँ कोई मानवीय दृष्टिकोण से भलाई की बात नहीं है। इस प्रकार यहाँ तीन प्रकार के दृष्टिकोण हैं। इसमें तो हमें प्रेम का नाटक ही वास्तव में भाता है। आनंद ही सभी कुछ का सच्चा हेतु है बाकी सब तो बुद्धि की व्याधियाँ हैं। और ये तभी तक चलती हैं जब तक हमारा प्रभु से सम्पर्क नहीं हो जाता। जैसे कि श्री कृष्णप्रेम कहते थे कि जहाँ 'वे' छू देते हैं वहीं मदोन्मत्त कर देते हैं। यह सौम्य चाल तभी तक रहती है जब तक 'उनकी' झलक नहीं मिल जाती। वह मिलने के बाद तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। तो गीता हमसे इस प्रकार के दिव्य कर्मों की माँग करती है।
मानव-कर्मों का संपूर्ण विस्तार क्षेत्र वह होना चाहिए जिसमें ईश्वरवेत्ता विचरण करेगा। उसकी सारी व्यक्तिगत और सामाजिक क्रिया, उसकी बुद्धि, हृदय और शरीर के सारे कर्म अब भी उसी के होंगे, पर अपने पृथक् व्यक्तिगत हेतु के लिए नहीं होंगे अपितु संसार में स्थित ईश्वर के लिए, सब प्राणियों में विराज रहे ईश्वर के लिए, और इसलिए कि वे सब प्राणी, स्वयं उसकी तरह ही, कर्ममार्ग द्वारा स्वयं अपने अन्दर विराजमान भगवान् की खोज की ओर आगे बढ़ें। संभवतः बाह्य रूप से उसके कर्म अन्य मनुष्यों के कर्मों से कोई मूल रूप से भिन्न प्रतीत न हों; युद्ध व शासन, शिक्षादान, और चिंतन, मनुष्य के मनुष्य के साथ जितने विभिन्न प्रकार के आदान-प्रदान हो सकते हैं वे सभी उसके कार्यक्षेत्र में हो सकते हैं, परंतु जिस भाव से वह इन कर्मों को करेगा वह अवश्य ही सर्वथा भिन्न होगा, और उसका वह भाव ही होगा जो अपने प्रभाव के कारण एक ऐसा महान् आकर्षण होगा जो लोगों को उसके अपने स्तर तक ऊपर खींचेगा, एक ऐसा महान् उत्तोलक (Lever) होगा जो मानवसमूह को उनके आरोहण में ऊँचा उठाएगा।
मुक्त मनुष्य के लिये भगवान् ने जो स्वयं का दृष्टांत रखा वह गंभीर रूप से सारगर्भित है; क्योंकि यह दृष्टांत दिव्य कर्मों के सम्बन्ध में गीता के सिद्धांत के सम्पूर्ण आधार को प्रकट कर देता है। मुक्त पुरुष वही है जिसने अपने-आपको दिव्य प्रकृति में उठा लिया है और उसी दिव्य प्रकृति के अनुसार सब कर्म करता है।..न तो कर्मप्रधान मनुष्य की कर्मण्यता और न संन्यासी, वैरागी या निवृत्तिमार्गी की कर्मविहीन ज्योति, न तो कर्मी मनुष्य का प्रचंड व्यक्तित्व और न तत्त्वज्ञानी ऋषि का उदासीन निर्व्यक्तित्व, इनमें से कोई भी संपूर्ण भागवत् आदर्श नहीं है। ये संसारी जन के तथा संन्यासी, या निवृत्तिमार्गी दार्शनिक के दो परस्पर विरोधी मानदण्ड हैं, जिनमें एक क्षर के कर्म में डूबे रहता है और दूसरा सर्वथा अक्षर की शान्ति में निवास करने का प्रयास करता है; परन्तु पूर्ण भागवत् आदर्श का उद्गम पुरुषोत्तम की उस प्रकृति से है जो इस परस्पर- विरोध के परे है और जो सभी भागवत् संभावनाओं में समन्वय साध देती है।
कर्मप्रधान मनुष्य किसी ऐसे आदर्श से संतुष्ट नहीं होता जो इस विश्वप्रकृति की, उस प्रकृति की त्रिगुणमयी क्रीड़ा की, मन-हृदय-शरीर के इस मानव-कर्म की परिपूर्णता पर अवलम्बित न हो।... क्योंकि यही उसकी प्रकृति, उसका धर्म है और वह किसी ऐसी चीज से किस प्रकार परिपूर्ण हो सकता है जो उसकी प्रकृति के लिए विजातीय हो? क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति से बँधा है और इस दायरे के अन्दर ही उसे अपनी पूर्णता को ढूँढ़ना होगा। हमारी मानव-प्रकृति के अनुसार ही हमारी मानव-पूर्णता हो सकती है; और इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उसके लिए अपने व्यष्टिधर्म अर्थात् स्वधर्म के अनुसार अपने जीवन और कर्म में यत्न करना चाहिए, जीवन और कर्म के बाहर नहीं। इस बात का गीता यह उत्तर देती है कि हाँ, इसमें भी एक सत्य है; मनुष्य के अन्दर ईश्वर की चरितार्थता, जीवन में भगवान् की लीला अवश्य ही आदर्श सिद्धि का एक अंग है। परन्तु यदि तुम उसे केवल बाहर ही ढूँढ़ो, जीवन में और कर्म के सिद्धान्त में, तो तुम उसे कभी नहीं पाओगे, क्योंकि तब तुम न केवल अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करोगे, जो अपने-आप में सिद्धि या पूर्णता का ही एक विधान है, परंतु सदा उसके गुणों के अधीन रहोगे - और यह असिद्धि का एक विधान है - सदा राग-द्वेष और सुख-दुःख के द्वंद्वों के अधीन रहोगे, विशेषतः प्रकृति के राजसिक गुण के वश हो जाओगे, कामना जिसका एक तत्त्व है और क्रोध, शोक और लालसा जिसके जाल हैं. - इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि अपूर्णता के इस अनादि कारण के अधिष्ठान हैं और फिर भी तुम इस इन्द्रिय-बोध, मन और बुद्धि में, निम्न प्रकृति की इस क्रीड़ा के दायरे में ही पूर्णता की खोज को रखना चाहते हो! यह प्रयास व्यर्थ है। तुम्हारी प्रकृति के क्रियात्मक पक्ष को पहले निवृत्ति की शान्ति को अपने अन्दर ले आना चाहिए; तुम्हें अपने-आपको इस निम्न प्रकृति से परे उठाकर उस तक ले जाना होगा जो तीनों गुणों से ऊपर है, जो परमतत्त्व में, आत्मा में प्रतिष्ठित है। केवल तभी जब कि तुम्हें वह आत्मप्रसाद लाभ होगा तुम एक मुक्त और भागवत् कर्म करने में समर्थ बन सकोगे।
इसमें बात एक ही है कि किसी भी मानसिक सूत्र से, या फिर किसी भी सूत्रबद्ध तरीके से, कोई भी योजना बनाकर, साधना का कोई भी कार्यक्रम बनाकर व्यक्ति दिव्य कर्म नहीं कर सकता। दिव्य कर्म तो तभी होंगे जब व्यक्ति भागवत् चेतना, पुरुषोत्तम की चेतना में निवास करेगा। क्योंकि अक्षर की चेतना में तो कर्म ही नहीं होंगे। जब व्यक्ति पुरुषोत्तम की चेतना से जुड़ जाएगा केवल तभी दिव्य कर्म होंगे। दिव्य कर्मों का अन्य कोई बाहरी मानदण्ड या कसौटी निर्धारित नहीं की जा सकती। क्योंकि उसमें तो व्यक्ति गुणों के अधीन ही रहता है। भगवान् की प्रेरणा से जो चीज आती है वह गुणों के अधीन नहीं है। वे तो गुणों के स्वामी हैं। बाकी तो शरीर की, प्राण की, मन की सभी चीजें, इच्छाएँ आदि सब तीनों गुणों के अधीन होती हैं, केवल भगवान् ही इनसे परे, इनसे मुक्त व इनके नियामक हैं। किन्तु जब व्यक्ति भगवान् से प्रेरणा प्राप्त कर उनकी ओर खुल जाता है तभी उसके कर्म दिव्य होंगे अन्यथा नहीं।
इसके विपरीत निवृत्तिमार्गी अथवा शान्तिमार्गी, संन्यासी ऐसी किसी सिद्धि की सम्भावना नहीं देखते जिसमें जीवन और कर्म का प्रवेश हो। (वे कहते हैं) क्या जीवन और कर्ममात्र ही बंधन और अपूर्णता का गढ़ नहीं है? क्या कर्म के स्वभावमात्र में अपूर्णता नहीं है जैसे अग्नि के साथ धुँआ पैदा करना जुड़ा है? क्या कर्म का सिद्धान्त ही अपने-आप में राजसिक नहीं है, कामना का जनक नहीं है, जो अपने-आप में ऐसा कारण है जिसके अवश्यंभावी परिणाम होते हैं ज्ञान का आच्छादन, उत्कट कामना तथा सफलता और विफलता के दौर, हर्ष और शोक में डोलते रहना, पुण्य और पाप के द्वन्द्व में फंसे रहना? परमेश्वर संसार में हो सकते हैं, पर वे संसार (तत्त्व) के नहीं हैं; वे त्याग के या निवृत्तिपरायण ईश्वर हैं, हमारे कर्मों के प्रभु या कारण नहीं; हमारे कमर्मों का स्वामी तो कामना है और कर्मों का कारण है अज्ञान। यदि यह जगत्, यह क्षर सृष्टि किसी अर्थ में भगवान् की अभिव्यक्ति या लीला कही भी जाए तो यह अज्ञ मूढ़ प्रकृति के साथ उनकी असिद्ध क्रीड़ा है, यह उनकी अभिव्यक्ति नहीं अपितु उनका तमाच्छादन ही है। और निश्चय ही संसार के स्वरूप पर प्रथम दृष्टिपात में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है और क्या जगत् का पूर्ण अनुभव हमें सदा ही इसी सत्य की शिक्षा नहीं देता? क्या यह अज्ञान का वह चक्र नहीं है जो जीव को कामना और कर्म की प्रेरणा के द्वारा तब तक बार-बार जन्मग्रहण के लिए बाँधता है जब तक कि अंत में इस प्रेरणा का क्षय न हो जाए या फिर इसे त्याग ही न दिया जाए? न केवल कामना ही, अपितु कर्म भी दूर हटा देना होता है; तभी निश्चल आत्मा में प्रतिष्ठित होकर जीव गतिहीन, कर्महीन, क्षोभहीन, केवल परंब्रह्म में जा सकेगा। गीता संसारी मनुष्य, क्रियाशील व्यक्ति की आपत्तियों की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्मवादी, निवृत्तिमार्गी की आपत्तियों का उत्तर देने पर अधिक ध्यान देती है। क्योंकि इस निवृत्तिमार्ग के पास एक उच्चतर और बलवत्तर सत्य होने परंतु फिर भी वह सत्य समग्र या परम सत्य न होने के कारण, इसका मनुष्य जीवन के विश्वव्यापी, पूर्ण और उच्चतम आदर्श के रूप में प्रचार परिणामतः अधिक संभावित रूप से मानव-जाति के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में एकांगी रूप से कर्मवाद के अनुसरण की भूल से उत्पन्न परिणामों की अपेक्षा कहीं अधिक भ्रामक और अनिष्ट करनेवाला हो सकता है। जब किसी प्रबल एकांगी सत्य को पूर्ण सत्य के रूप में स्थापित किया जाता है तो उसका प्रकाश बहुत तीव्र होता है, पर साथ ही उससे बहुत तीव्र संकर या विभ्रम भी होता है; क्योंकि उसमें जो सत्यांश है उसकी तीव्रता ही उसके त्रुटि के तत्त्व को बढ़ानेवाली होती है। कर्मवादी आदर्श की त्रुटि मानवजाति को एक ऐसी दिशा में पूर्णता के अनुसंधान के लिए प्रवृत्त कर सकती है जहाँ पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती और इस प्रकार अज्ञान की अवधि को केवल लंबा कर देती है और मानव प्रगति में गतिरोध पैदा कर देती है; परन्तु निवृत्तिमार्ग के आदर्श में जो भूल है उसमें तो संसार के विध्वंस का ही तत्त्व निहित है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि यदि इस आदर्श को सामने रखकर मैं कर्म करूँ तो मैं इन सब प्राणियों को नष्ट करने वाला और विभ्रम का कारण बनूँगा। यद्यपि किसी व्यष्टि-पुरुष की मूल, चाहे वह देवतुल्य पुरुष ही क्यों न हो, सारी मानवजाति को नष्ट नहीं कर सकती तथापि उससे कोई ऐसा विस्तृत संभ्रम पैदा हो सकता है जो अपने स्वभाव से ही मानवजीवन के आधार को नष्ट करने वाला और उसकी उन्नति के सुनिश्चित क्रम को बिगाड़नेवाला हो।
इसलिए मनुष्य के अन्दर जो निवृत्तिपरक झुकाव है उसे अपनी अपूर्णता का भान होना चाहिए और प्रवृत्तिपरक झुकाव के पीछे जो सत्य है, - वह सत्य है मनुष्य के अन्दर भगवान् की चरितार्थता और मानवजाति की सभी क्रियाओं में भगवान् की उपस्थिति - उसे भी स्वीकार कर अपनी बराबरी का स्थान देना होगा। भगवान् केवल नीरवता में ही नहीं हैं, कर्म में भी हैं। प्रकृति से अप्रभावित उदासीन (निष्कर्म) पुरुष की निवृत्ति, और कर्मप्रधान पुरुष की प्रवृत्ति, जो अपने-आपको प्रकृति के हवाले कर देता है ताकि यह महान् विश्व-यज्ञ, पुरुष-यज्ञ संपन्न हो सके ये दोनों निवृत्ति और प्रवृत्ति - कोई ऐसी चीजें नहीं हैं मानो सतत् संग्रामरत यथार्थता और मिथ्यात्व हों, अथवा यह भी नहीं है कि ये दोनों परस्पर विरोधी यथार्थताएँ हों, जिनमें से एक श्रेष्ठ और दूसरी कनिष्ठ है और दोनों एक-दूसरे के लिये घातक हों; अपितु ये तो भागवत् अभिव्यक्ति की द्विविध शर्तें हैं। अक्षर अकेला ही इनकी परिपूर्णता की कुंजी या परम रहस्य नहीं है। इन दोनों की परिपूर्णता को, इनके समन्वय को पुरुषोत्तम भाव में खोजना होगा जो यहाँ श्रीकृष्णरूप से उपस्थित हैं, जो एक ही साथ परमपुरुष, जगदीश्वर तथा अवतार हैं। भगवान् की प्रकृति में प्रवेश कर के दिव्यीकृत मानव उसी तरह कर्म करेगा जैसे वे करते हैं; वह अपने को अकर्म में नहीं छोड़ देगा। भगवान् अज्ञानमय व्यक्ति और ज्ञानी पुरुष दोनों ही में कार्यरत हैं... क्योंकि वे ही अपनी शक्ति के तरीकों और मानदण्डों में कर्म करते हैं; प्रकृति की प्रत्येक गति, जिस प्राणीजगत् को वे रचते हैं उसका प्रत्येक अणु उन्हीं की उपस्थिति से व्याप्त है, उन्हीं की चेतना से परिपूर्ण है, उन्हीं के संकल्प से प्रेरित है, उन्हीं के ज्ञान से रूपायित है।
यहाँ मुख्य बात यह है कि दो परस्पर विरोधी मत हैं। एक साधारण मत तो यह है कि यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसका काम ही नहीं चलेगा क्योंकि बिना कर्म किये उसकी कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार होगी। इसलिए व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा, अपनी कामना-पूर्ति करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इच्छाओं और कामनाओं से ही सारा संसार चल रहा है और इसी तरह चलेगा क्योंकि बिना इच्छाओं और कामनाओं के मनुष्य कैसे रह सकते हैं। इसलिए अधिकांश लोग इनकी पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं। आदर्श के लिए कर्म करने वाले मनुष्य तो बहुत ही कम मिलेंगे। और इससे भी कम इस स्थिति पर पहुँचने वाले लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि वे भगवान् की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। अधिकांश मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं। इससे अलग एक दूसरा मत निवृत्तिमार्गियों का है जो कहते हैं कि साधारणतया अधिकांश मनुष्य माया के ही चक्कर में फंसे रहेंगे, द्वंद्वों में ही रहेंगे और तीनों गुणों से प्रभावित होते रहेंगे। उसका कोई ओर-छोर नहीं है क्योंकि वे अज्ञानमय जीव हैं और अज्ञान में ही जीवन व्यतीत करते रहेंगे। किन्तु परमात्मा की ओर जानेवाला व्यक्ति कामनाओं और इच्छाओं के द्वारा कोई कर्म नहीं करता। परन्तु इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी संकल्प कर ले कि वह बिना कामना के कर्म करेगा, तो भी कर्म के अंदर कामना तो किसी प्रकार घुस ही जाती है। इन द्वंद्वों से, गुणों से मुक्त होकर कर्म करना संभव ही नहीं है।
इसलिये निवृत्तिमार्गियों का यह दृष्टिकोण है कि बिना कामना के कर्म हो ही नहीं सकते, उनमें कामना तो घुस ही जाएगी। अतः भगवान् के साथ युक्त होने के लिए, ज्ञान में जाने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है कि व्यक्ति इन चीजों को कम-से-कम कर दे और अन्त में इन्हें समाप्त ही कर दे। इसलिए उनके द्वारा जो समाधान दिया गया है वह है अकर्म। उनके अनुसार व्यक्ति अक्षर पुरुष की दिव्य चेतना में रहकर, सबसे अप्रभावित होकर समता में निवास करे। जिसमें कर्म करने की कोई वृत्ति है ही नहीं क्योंकि उनके अनुसार व्यक्ति कर्म तो किसी फल की आशा से तथा अज्ञान के कारण करता है। इस प्रकार ये दो मत हैं।
श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि गीता के अनुसार साधारण सांसारिक मनुष्यों का मत तो इतना मूढ़ता और अज्ञान का है कि उसकी समस्या तो स्पष्ट ही दिखाई देती है, उसे अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। पर जो इन निवृत्तिमार्गियों, ज्ञानियों, संन्यासियों का मत है गीता उसे ही अधिक संबोधित करती है। क्योंकि वह ही घातक दृष्टिकोण है। उसमें सांसारिक मत से बड़ा एक सत्य है। मनुष्य देखता है कि वह भगवान् की ओर अग्रसर हो रहा है, और इस उद्देश्य के सामने वह अन्य सभी चीजों को अनदेखा कर देता है, उन्हें गौण महत्त्व प्रदान करता है। इससे ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए गीता इसे अधिक संबोधित करती है।
तब फिर इसका उपाय क्या है? इसके लिए गीता में भगवान् ने स्वयं का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि निवृत्तिमार्गी कहते हैं कि बिना कामना के कर्म नहीं हो सकता जबकि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है और मुझे कोई भी कामना नहीं है फिर भी मैं कर्म करता हूँ क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो लोक-संग्रह नहीं होगा और लोग नष्ट हो जाएँगे। यदि व्यक्ति यह मान ले कि यह जो अभिव्यक्ति है वह भगवान् की भूल या बेवकूफी मात्र नहीं है बल्कि यह उनकी परिकल्पना है, उन्हीं का नक्शा है और वे इसके पीछे उनका कोई महत् उद्देश्य है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, और वे जो कुछ करना चाह रहे हैं वह अभी तक संसिद्ध नहीं हुआ है। यदि हम इस प्रकार सोचें तो फिर एक दूसरा दृष्टिकोण प्राप्त होता है। उसी उद्देश्य को संसिद्ध करने के लिए भगवान् संत के रूप में, महात्मा के रूप में, विभूति के रूप में, अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। और यहाँ गीता स्वयं उसकी घोषणा कर रही है कि उनके कर्म किस प्रकार के हैं। प्रतीति में लगता है कि भगवान् के कर्म भी तीनों गुणों से लिप्त हैं, परन्तु वास्तव में वे गुणों से लिप्त नहीं हैं। हमारी संस्कृति में परंपरा से यह मान्यता है कि भगवान् चिन्मय हैं। गुण उन्हें छू भी नहीं सकते। प्रतीति में हमें उनके कर्म गुणों के अधीन लग सकते हैं क्योंकि हमें इस सब के पीछे के उद्देश्य का पता नहीं होता। परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक, प्राणिक, भौतिक प्रकृति के अधीन होकर और उसी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर के कर्म करता है तो उसके कर्म त्रिगुणमय ही होंगे। इनसे बचा ही नहीं जा सकता। परन्तु जब इनसे परे आत्मा की सत्ता, जो कि तीनों गुणों से परे है, जो प्रकृति की चीज नहीं है, से प्रभावित होकर अथवा उससे प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म करता है तो ऐसे में भले ही किसी दूसरे को ऐसा लग सकता है कि वह सत्त्व, रज या तम से प्रभावित है और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन आ सकते हैं, परन्तु सब कुछ के बावजूद वह रहता तो गुणों से ऊपर ही है। वह उनसे प्रभावित नहीं है। न तो वह द्वंद्वों से प्रभावित होता है और न ही गुणों से। वास्तव में तो कहीं भी गुण तो हैं ही नहीं, केवल प्रतीति ही है क्योंकि भगवान् की परा प्रकृति ही सब कुछ करती है। गुण तो हमें केवल हमारी मानसिक चेतना के वर्तमान गठन के कारण दिखाई देते हैं। इसलिए जब कोई अवतार या फिर भगवान् को समर्पित कोई व्यक्ति कर्म करता है तो भले ही हमें दिखाई न पड़े, परन्तु उसके कर्म मुक्त और दिव्य होते हैं। तो फिर दिव्य कर्म का आधार क्या है? वास्तव में इसका आधार है व्यक्ति का परमेश्वर, पुरुषोत्तम के साथ जुड़ाव होना। इसीलिए भगवान् श्रीकृष्ण अब सतत् रूप से, अधिक-से-अधिक यह कहते जाएँगे कि 'मेरी' ओर मुड़, 'अहम्', 'माम्'। क्योंकि इसके बिना कर्म करने का तो कोई सच्चा आधार ही नहीं है। यदि पुरुषोत्तम की स्थिति न हो तो दिव्य कर्म संपादित हो ही नहीं सकते। या तो कर्म होंगे इच्छाओं से, अज्ञान से, कामनाओं से, अहम् से, या फिर व्यक्ति की स्थिति मुक्ति की या अकर्म की होगी। अक्षर ब्रह्म से एक होने के बाद कर्म न्यूनतम ही होंगे और जब शरीर छूट जायेगा तो वे बचे-खुचे कर्म भी छूट जायेंगे, जैसी कि ज्ञानमार्गियों की शिक्षा है। गीता इस रहस्य को अब विकसित करेगी।
अब आगे जाने से पहले गीता ने पहले बात की कि तुझे कर्म का अधिकार है, कर्मफल का नहीं 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'। इसलिए व्यक्ति यह सोचता है कि कर्म तो वह कर ही सकता है। यहाँ पहले तो यह बता दिया गया कि हमें कर्म से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। परन्तु अब आगे गीता यह बताने वाली है कि कर्म तो व्यक्ति कर ही नहीं सकता। कर्म तो भगवान् की प्रकृति ही करती है। मनुष्य तो अपने अहम् के कारण कत्र्तापन को अपने ऊपर आरोपित करता है कि 'मैं कर रहा हूँ'। परन्तु वास्तव में तो कर्म तो प्रकृति ही कर रही है।
III. प्रकृति का नियतिवाद
कुछ लोगों द्वारा उन श्लोकों को, जिनमें गीता ने अहमात्मक जीव के प्रकृति के वशीभूत होने पर बल दिया है, इस प्रकार समझा गया है मानो वे एक ऐसे निरपेक्ष-निरंकुश और यांत्रिक नियतिवाद का प्रतिपादन हैं जो वैश्विक अस्तित्व में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। निश्चय ही उन श्लोकों की भाषा बहुत ही प्रभावशाली है, और सुनिश्चित अथवा निरपेक्ष प्रकार की प्रतीत होती है। परन्तु अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी, गीता के विचार को उसके समग्र रूप में ग्रहण करना चाहिए और किसी एक अभिपुष्टि या कथन को, अन्य कथनों के साथ के संबंध से सर्वथा अलग कर के, अपने-आप में सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। जैसा कि, वास्तव में प्रत्येक सत्य, भले वह अपने-आप में कितना ही यथार्थ क्यों न हो, अन्य सत्यों से, जो उसे मर्यादित करते हुए भी परिपूर्ण करते हैं, अलग कर दिया जाए तो बुद्धि को फँसानेवाला एक फंदा और मन के लिए भ्रामक मत बन जाता है; क्योंकि वास्तव में प्रत्येक सत्य एक जटिल ताने-बाने का एक सूत्र है (उसका एक अंग है) और किसी भी सूत्र को उस समग्र ताने-बाने से अलग कर के नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार गीता में सभी कुछ आपस में एक-दूसरे से इस प्रकार गहनता से गुंथा हुआ है कि उसको हर बात को संपूर्ण कलेवर के साथ मिलाकर ही समझना चाहिए... हमारी जटिल सत्ता के एक छोर पर प्रकृति के साथ जीव के सम्बन्ध का एक ऐसा पहलू है जिसमें जीव एक प्रकार से पूर्ण स्वतंत्र है; दूसरे छोर पर दूसरा पहलू है जिसमें एक प्रकार से प्रकृति का कठोर नियतिवाद है; इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता का एक आंशिक और दिखावटी, और इसलिए एक अवास्तविक आभास भी होता है जिसे जीव अपने विकसनशील मन के अन्दर इन दो विरोधी छोरों के विकृत प्रतिबिंब के द्वारा ग्रहण करता है। हम स्वतंत्रता के इस आभास को ही न्यूनाधिक भूल के साथ, स्वतंत्र-इच्छा कहा करते हैं; परन्तु गीता पूर्ण मुक्ति और प्रभुत्व को छोड़कर और किसी चीज को स्वतंत्रता नहीं मानती।
हमें यहाँ एक सावधानी रखने की हिदायत दी गई है कि गीता के श्लोकों को उसके पूर्ण स्वरूप से अलग-थलग कर के एकांगी रूप से नहीं लेना चाहिए। इसके श्लोकों से यह अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिये कि केवल प्रकृति का अंकुश या नियम चलता है और स्वतंत्र इच्छा का कोई स्थान नहीं है। यह तो गीता के श्लोकों का अतिशय अर्थ लगाना हुआ।
अब, दो मत प्रचलित हैं। एक मत यह है कि सब कुछ पूर्वनिर्धारित है और जैसा भाग्य में लिखा होता है वैसा ही होता है। दूसरा मत है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और चाहे जैसे भी कर सकता है। व्यावहारिक रूप में व्यक्ति देखता है कि किसी-किसी विशिष्ट क्षण में प्रत्यक्ष रूप से यह महसूस होता है कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह यह भी कर सकता है, वह भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि वह ऐसा न कर सके। उदाहरण के लिए हम इस पेंसिल को इधर भी रख सकते हैं और उधर भी रख सकते हैं। यदि इस तरीके से देखा जाए तो स्वतंत्रता तो है ही। परन्तु जब व्यक्ति अपने अंदर अवलोकन करता है तो वह देखता है कि यह स्वतंत्रता की प्रतीति मात्र है, वास्तव में सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। व्यक्ति के अंदर जो विचार आते हैं, उत्प्रेरणाएँ आदि आती हैं, वे किसी उच्चतर स्थान से पूर्वनिर्धारित होती हैं। वास्तव में जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से, अपने ब्रह्म रूप से तादात्म्य में होता है तभी वह यथार्थतः स्वतंत्र है। परन्तु जब व्यक्ति भौतिक तत्त्व से, जड़तत्त्व से तादात्म्य में है तब वह पूर्ण रूप से उसका दास होता है। क्योंकि फिर एक निश्चित नियमों के आधीन रहकर ही काम होगा। बीच की स्थिति में व्यक्ति को स्वतंत्रता का भान होता है। इसको मानने वाले लोग कह देते हैं की स्वतंत्रता का आभास केवल एक बोध है अन्यथा तो भगवान् ने सब कुछ निर्धारित ही कर रखा है। श्रीअरविन्द का कहना है कि स्वतंत्रता का यह भान भ्रम नहीं है। वास्तव में व्यक्ति को स्वतंत्रता तो है, परंतु स्वतंत्रता के इस भाव को हम गलत स्थान पर अर्थात् अहं पर आरोपित कर देते हैं। अपने-आप का अर्थ जब व्यक्ति अपने बाहरी व्यक्तित्व से मान बैठता है, अपने शरीर, विचार तथा भावनाओं आदि से मान बैठता है, तो उस भाग को स्वतंत्रता नहीं है। व्यक्ति के अन्दर कोई ऐसी चीज है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके कारण ही व्यक्ति को स्वतंत्रता का आभास होता है जिसे वह गलती से अपने अहं पर, बाहरी व्यक्तित्व पर अध्यारोपित करने की भूल करता है।
वास्तव में, स्वतंत्रता और नियति एक ही वस्तु के केवल दो पक्ष हैं क्योंकि मूलभूत सत्य है विश्व का आत्मनिर्धारण तथा उसके अंदर व्यक्ति का गुह्य आत्मनिर्धारण। कठिनाई इस बात से उठती है कि हम अज्ञान के ऊपरी मन में निवास करते हैं, यह नहीं जानते कि पीछे की ओर क्या हो रहा है और प्रकृति के केवल बाह्य क्रिया-व्यापार की प्रक्रिया को देखते हैं। वहाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता तथ्य है प्रकृति की एक अदम्य नियति और चूंकि हमारी सतही चेतना उस प्रक्रिया का अंग होती है, इसलिए हम उस द्विपक्षीय सत्य के दूसरे पक्ष को देखने में असमर्थ होते हैं। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिये, ऊपरी तल पर जड़तत्त्व के अंदर एक प्रकार की पूर्ण नियति है - यद्यपि विज्ञान की नवीनतम शाखा द्वारा अब इस पर आपत्ति जताई जाती है। जब प्राण का प्रादुर्भाव होता है तो एक प्रकार की नमनीयता का भी प्रवेश होता है और इसके कारण ठीक-ठीक उसी तरह किसी चीज का पूर्वानुमान कर पाना कठिन हो जाता है जिस तरह हम एक कठोर नियम का अनुसरण करने वाली भौतिक जड़वस्तुओं के विषय में पूर्वकथन करते हैं। यह नमनीयता मन के विकास के साथ और बढ़ जाती है और इस कारण मनुष्य को कम-से-कम स्वतंत्र-इच्छा का, अपने कर्म के चुनाव का तथा स्वेच्छापूर्वक गति करने का एक प्रकार का भान हो सकता है जो कम-से-कम परिस्थितियों को निर्धारित करने में सहायक होता है। परंतु यह स्वतंत्रता संदेहास्पद है, क्योंकि इसे एक प्रकार का भ्रम, प्रकृति का एक उपाय, उसके नियति-रूपी यंत्र का ही एक अंग घोषित किया जा सकता है, यह केवल प्रतीत होती स्वतंत्रता है या फिर अधिक-से-अधिक एक सीमित, सापेक्ष और अधीनस्थ स्वतंत्रता है। जब मनुष्य पीछे की ओर, प्रकृति से दूर, पुरुष के समीप जाता है और ऊपर की ओर, मन से दूर, आध्यात्मिक आत्मतत्त्व तक चला जाता है केवल तभी स्वतंत्रता का पक्ष सर्वप्रथम प्रत्यक्ष होता है और फिर, उस दिव्य संकल्प के साथ, जो कि प्रकृति से ऊपर है, एकत्व होने पर, पूर्ण होता है।
यदि व्यक्ति श्रीमाँ की इच्छा के साथ एक हो जाता है तो पूर्ण स्वतंत्रता है। यदि जड़तत्त्व के साथ एक होता है तो पूर्ण दासता है। बीच-बीच में दोनों का मिश्रण है। यही जीवन का सार है। वास्तव में मोटा-मोटा रूप तो यही है कि हमें स्वतंत्रता का आभास हो सकता है परन्तु वास्तविक स्वतंत्रता तो श्रीमाँ के साथ एक होने पर ही आ सकती है।
यहाँ इस जगत् की सभी वस्तुएँ एक एवं अखंड नित्य विश्वातीत और विश्वमय ब्रह्म हैं जो कि दिखने में विभिन्न वस्तुओं और प्राणियों के रूप में विभक्त हुआ प्रतीत होता है; परंतु ऐसा केवल प्रतीति में ही है, क्योंकि वास्तव में वह सभी पदार्थों और प्राणियों में सदा ही एक तथा 'सम' है और भिन्नता तो केवल ऊपरी दृष्टिगोचर वस्तु है। जब तक हम अज्ञानमय प्रतीति में रहते हैं तब तक हम 'अहं' हैं और प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। बाह्य प्रतीतियों के दास बने हुए, द्वंद्वों से बँधे हुए और शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य, हर्ष-शोक, सुख-दुःख, सौभाग्य-दुर्भाग्य एवं जय-पराजय के बीच ठोकरें खाते हुए हम लाचार हो माया के पहिये के लोहमय या स्वर्णलोहमय घेरे पर चक्कर काटते रहते हैं। अधिक-से-अधिक हमारे पास केवल अत्यन्त तुच्छ और सापेक्ष स्वतंत्रता ही होती है जिसे कि हमारे द्वारा अज्ञानपूर्वक अपनी स्वतन्त्र इच्छा कहा जाता है। पर मूलतः वह मिथ्या होती है, क्योंकि प्रकृति के गुण ही हमारी व्यक्तिगत इच्छा में से अपने-आपको व्यक्त करते हैं; प्रकृति की शक्ति ही हमें वश में रखती हुई, पर हमारी समझ और पकड़ से बाहर रहकर यह निर्धारित करती है कि हम क्या इच्छा करेंगे और वह इच्छा किस प्रकार करेंगे। हमारा स्वतन्त्र अहं नहीं, अपितु प्रकृति यह चुनाव करती है कि अपने जीवन की किसी भी घड़ी में हम, भले ही एक युक्तियुक्त संकल्प द्वारा या विचाररहित आवेग के द्वारा, किस पदार्थ या हेतु की अभिलाषा करेंगे।.... सर्वदा हो इस निम्न प्रकृति के जाल में पड़े होने पर भी स्वतंत्रता की मिथ्या धारणा के अज्ञान का बोध हो वह दृष्टिबिंदु है जो गीता का निष्कर्ष है और इस अज्ञान का खण्डन करने के लिए ही गीता अहमात्मक जीव की इस जगत् में गुणों के प्रति पूर्ण वश्यता बताती है।
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।। २७।।
२७. जबकि कर्म पूर्णतया प्रकृति के गुणों के द्वारा किये जाते हैं, जिसका मन अहंकार से विमूढ़ हो गया है वह मानता है कि मैं ही उनका करनेवाला हूँ।
....व्यष्टिगत जीव के रूप में मनुष्य, कर्म और भूतभाव (अपने होने के भाव) के साथ अपने अज्ञानवश तादात्म्य के कारण मानो वे कर्म और उसका भूतभाव उसकी संपूर्ण आत्मा ही हैं न कि ये केवल उसकी आत्मा की एक शक्ति हैं - अहंकार-विमूढ़ हो जाता है। वह सोचता है कि स्वयं वह और दूसरे लोग ही सब कुछ कर रहे हैं; वह यह नहीं देख पाता कि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है और यह कि अज्ञान तथा आसक्ति के कारण वह प्रकृति के कर्मों को अपने लिए गलत ढंग से प्रस्तुत करता है और विकृत करता है। वह गुणों द्वारा दास बनाकर रखा हुआ है, कभी वह तमोगुण की जड़ता में फँस जाता है, कभी रजोगुण की प्रचंड आँधियों में उड़ा लिया जाता है और कभी सत्त्वगुण के आंशिक प्रकाशों में उसे सीमित कर दिया जाता है और वह अपने-आप को बिल्कुल भी अपने प्राकृत मन से अलग नहीं देख पाता जिसमें गुणों द्वारा फेर-बदल होता रहता है। इसीलिए वह सुख और दुःख, हर्ष और शोक, काम और आवेग, आसक्ति और जुगुप्सा द्वारा वशीभूत कर लिया जाता है, उसे जरा भी स्वतंत्रता नहीं रहती।
यहाँ मूलभूत बात यह है कि इस ब्रह्माण्ड में परमात्मा की आद्याशक्ति के संकल्प के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। यदि यह बात न हो तो सारी अभिव्यक्ति, सारा ब्रह्माण्ड निरर्थक ही हो जाएगा। वास्तव में उस आद्याशक्ति के अतिरिक्त कोई भी कुछ भी नहीं करता, केवल वही कर्जी है। इसके अतिरिक्त यदि हमें और कुछ दिखाई देता है तो वह घोर अंधकार है, क्योंकि यह तो एक परम सत्य है कि वही एकमात्र कीं है। यदि हमें यह सत्य नहीं दिखाई देता तो हम मूढ़ हैं। व्यक्ति को जो निम्न प्रकृति और गुण दिखाई देते हैं वह तो केवल एक देखने का तरीका मात्र है। वास्तव में तो केवल एक ही प्रकृति है जो क्रिया करती है। श्रीमाँ की चेतना पर हमारा जो प्रतिबिंबन (reflection) है वह हमें निम्न प्रकृति और गुणों का आभास कराता है। अब गीता इसी में जा रही है कि व्यक्ति को निम्न प्रकृति और गुणों का आभास क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि हमने अपने-आप को एक अहम् पर केन्द्रित कर रखा है और इस तरह से हम एक कारागार में बंद हैं और उसी के दृष्टिकोण से सारे ब्रह्माण्ड को देखते हैं। और इसी कारण हमें दूसरे व्यक्ति, जीव, चीजें आदि नजर आते हैं। वास्तव में तो यहाँ पर सर्वत्र केवल एक आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं। अहम् में भी हमारी चेतना के तीन पर्दे हैं - मन, प्राण और शरीर। चेतना का प्रतिबिंब (reflection) जिस पर्दे पर जितना पड़ेगा उसके अनुसार हमारा कर्म सात्त्विक, राजसिक या तामसिक होगा। क्योंकि क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ तो सारी वहीं से ही निर्धारित होती हैं, हमें तो केवल उनका अहसास होगा। जिस व्यक्ति को थोड़ा बोध होगा वह बता सकेगा कि सात्त्विक, राजसिक और तामसिक में से वह किस रूप में कार्य कर रहा है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति को यह पता हो कि कौनसा कर्म प्रधानतः सात्त्विक है, कौनसा राजसिक और कौनसा तामसिक। क्योंकि सात्त्विक, राजसिक अथवा तामसिक का अहसास हमें इसलिए होता है क्योंकि हम सभी चीजों को उस प्रतिबिंबन (reflection) से देखते हैं और इसी कारण हमें क्रिया-प्रतिक्रिया और कार्य-कारण की कड़ियाँ नजर आती हैं। जबकि यह तो केवल व्यक्ति का एक बोध होता है। गीता कहती है कि व्यक्ति का इस तरीके का बोध मूढ़ता का है कि वह कोई कर्म कर रहा है अथवा कोई गुण कार्य कर रहे हैं, यह तो उसका कोई विषय ही नहीं है क्योंकि ये सब तो केवल प्रकृति ही करती है। यदि हम परमात्मा के साथ तदात्म हैं तो प्रकृति हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है अन्यथा हम प्रकृति के हाथों में एक खिलौने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। इसी बात को गीता निर्णायक रूप में कहती है। यदि हम यह सोचते हैं कि हमें पूरी स्वतंत्रता है और हम स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकते हैं अथवा चयन कर सकते हैं तो यह केवल हमारा भ्रम है। क्योंकि हम अपने विचारों में, भावनाओं में, आवेगों में अथवा अवचेतना से जो कुछ उठता है उसके अनुसार कार्य करने को बाध्य होते हैं। 'दिव्य संकल्प' को जो काम कराना होता है वह उसी प्रकार की उत्प्रेरणाएँ, विचार, कामनाएँ, प्राणिक आवेग आदि हमारे अवचेतन में से उत्पन्न कर लेता है और उसी के अनुसार हम क्रिया करने को बाध्य होते हैं। भय, उत्कण्ठा, कामना, भावनात्मकता, अभीप्सा आदि जिसकी जब जितनी आवश्यकता होती है वे उतने ही उठ जाते हैं और हम वही कार्य करने लगते हैं, इसी प्रकार वहीं से सभी कुछ निर्धारित होता है। और हमें यह लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, जबकि हम स्वयं वास्तव में कुछ नहीं कर रहे होते। हम तो प्रकृति के हाथों में केवल एक यंत्र होते हैं। इस सारी प्रक्रिया का उद्देश्य है कि प्रकृति क्रमविकास के माध्यम से धीरे-धीरे भगवान् को हमारे भीतर जागृत करना चाहती है। इसीलिए गीता कहती है कि साक्षी, अनुमता, भर्ता, भोक्ता, ज्ञाता और ईश्वर - उत्तरोत्तर बढ़ते हुए ये छः भाव व्यक्ति प्रकृति के प्रति अपना सकता है। सबसे पहले व्यक्ति अहं से बद्ध होता है जिसमें वह संसार के चक्र में, सुख-दुःख, हानि-लाभ, शोक-हर्ष, सफलता-असफलता आदि नाना प्रकार के द्वंद्वों में अथवा इसमें कि मेरी अमुक क्षमताएँ हैं और मैं कुछ कर सकूँगा, फंसा रहता है जबकि ये सब व्यक्ति की प्रतिक्रियाएँ हैं जिनसे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो जैसे होना है वह वैसे ही होता है। व्यक्ति की योजनाओं से कुछ नहीं होता। उससे तो केवल एक निजी आत्मपरक जगत् का निर्माण, एक मानसिक, प्राणिक रचना हो जाती है जिसमें व्यक्ति रहने लगता है और इस प्रकार धीरे-धीरे इस अज्ञान में उसका क्रमविकास चलता रहता है। इसलिए आत्म-प्रभुत्व की तरफ चलने के लिये पहला काम है कि इस चक्र में न उलझ कर व्यक्ति उससे अलग हट कर यथा-क्षमता अवलोकन करे तो यह खेल थोड़ा-थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाता है। जब हम इस चक्र में फंसे रहते हैं, अपने आवेगों और विचारों के अनुसार काम करते हैं तो हमें यह खेल समझ में नहीं आ सकता। जैसे कि कोई खेल चल रहा हो तो उसमें भाग लेने वाला व्यक्ति वह सब चीज नहीं देख पाएगा जो अलग खड़ा व्यक्ति देख सकेगा। इसलिये पहला है साक्षी भाव। फिर जैसे-जैसे यह भाव विकसित होगा और ज्यों-ज्यों हम ऊपर उठेंगे त्यों-त्यों हम देखेंगे कि प्रकृति का जो यह सारा कार्य-व्यापार चल रहा है उसमें व्यक्ति की भीतर से कोई-न-कोई अनुमति अवश्य है अन्यथा ये सब काम चल ही नहीं सकते थे। यह आभास व्यक्ति को होने लगता है। तो यह है अनुमंता का स्तर। और उसके बाद में फिर अनुभव होगा कि इन सब कर्मों के लिए प्रकृति अपनी सारी ऊर्जा भी हम से ही प्राप्त कर रही है अन्यथा तो वह क्रिया कर ही नहीं सकती, हम ही अनुमंता और भर्ता हैं। इससे और अधिक गहराई में जाने पर हम यह पाएँगे कि प्रकृति यह सब हमारी अपनी प्रसन्नता, हमारे भोग के लिये कर रही है, यह सब समीकरण तो हमारे अपने भोग के लिए ही बनाया गया है। हम ही इसके भोक्ता हैं। इससे और आगे जाने पर जब व्यक्ति अपनी सतही प्रकृति से हटकर अपने सच्चे स्वरूप पर पहुँच जाता है तो सब कुछ का उद्देश्य समझ में आ जाता है कि यह सब क्यों हो रहा है, और इस सारे खेल का कथानक समझ में आ जाता है। यह है ज्ञाता का स्तर । उससे और भीतर जाने पर ईश्वर भाव प्राप्त होता है और व्यक्ति को यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि प्रकृति यह सब कार्य-व्यापार करती ही केवल उसकी प्रसन्नता के लिये है। इसके अतिरिक्त वह और कुछ करती ही नहीं। परंतु प्रकृति जिस 'मैं' की प्रसन्नता के लिये काम करती है वह वह सतही प्रकृति का 'मैं' नहीं है जो हम अपने को सामान्यतया मानते हैं। यह तो केवल एक ऊपर का आवरण-मात्र है। इस प्रकार ये छः स्तर हैं। ईश्वर का भाव तो जीव के लिये ग्रहण करना मुश्किल है। वह तो अवतारों में ही आता है। परन्तु बहुत हद तक व्यक्ति इसके निकट जा सकता है। गीता यह घोषणा करती है कि जो भी व्यक्ति यह सोचता है कि वह कोई कर्म करता है और वह कुछ चयन कर सकता है तो यह सब उसकी मूर्खता है। समस्त कर्म तो भगवान् की प्रकृति ही करती है।
[प्रकृति के नियतिवाद का अर्थ है]...कि जिस अहंकार के द्वारा हम क्रिया करते हैं वह स्वयं भी प्रकृति की क्रिया का एक यंत्र है और इसलिए प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकता; अहंकार की इच्छा प्रकृति द्वारा निर्धारित इच्छा है, यह उस प्रकृति का एक अंग है जो अपने पूर्व कर्मों और परिवर्तनों के द्वारा हमारे अन्दर गठित हुई है और इस प्रकार गठित प्रकृति में जो इच्छा है वही हमारे वर्तमान कर्म का निर्धारण करती है।... हम ऐसे बोलते और क्रिया करते हैं मानो किसी भी क्षण विशेष में हम अपने साथ जो चाहें वैसा करने में एक पूर्ण आंतरिक चयन की स्वच्छंदता रखते हों। परन्तु ऐसी कोई पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है, हमारे चयन के लिए ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है।
निश्चय ही हमारी इच्छा को सदा ही किन्हीं प्रस्तुत संभावनाओं में से कुछ चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि इसी तरीके से प्रकृति सर्वदा क्रिया करती है; यहाँ तक कि हमारी निश्चेष्टता, किसी प्रकार की इच्छा करने से हमारी अस्वीकृति भी एक चुनाव है, प्रकृति की हममें जो इच्छा-शक्ति है वह उसी की एक क्रिया है; परमाणु तक में भी एक इच्छा-शक्ति सदा अपनी क्रिया करती रहती है। सारा अन्तर केवल इसमें है कि किस हद तक हम प्रकृति की इस इच्छा-शक्ति की क्रिया के साथ अपने स्वत्व के या स्वयं के कर्तृत्व के भाव को जोड़ते हैं। जब हम इस प्रकार अपने-आपको उसके साथ जोड़ लेते हैं तब यह सोचने लगते हैं कि यह इच्छा हमारी है और यह कहने लगते हैं कि यह एक स्वाधीन इच्छा है, हम ही कर्ता हैं....
[तो भी स्वतंत्र-इच्छा का बोध....निरा भ्रम नहीं है, यह केवल दृष्टिकोण और नियोजन की ही भूल है। अहंकार समझता है कि वही सच्ची आत्मा या मूलतत्त्व है और इस प्रकार कर्म करता है मानो वही कर्म का वास्तविक केन्द्र हो और मानो सब कुछ उसी की तुष्टि के लिए है और यहीं वह दृष्टिकोण और नियोजन की भूल करता है। ऐसा सोचना गलत नहीं है कि हमारे अन्दर, हमारी प्रकृति की इस क्रिया में कोई चीज या कोई पुरुष ऐसा है जो हमारी प्रकृति के कर्म का वास्तविक केन्द्र है और सब कुछ उसी के लिये है; परन्तु वह केन्द्र अहंकार नहीं है, अपितु हृदयों में निगूढ़ ईश्वर हैं और वह दिव्य पुरुष और जीव है जो अहंकार से पृथक् दिव्य पुरुष की सत्ता का ही एक अंश है। अहं-बोध का स्वाग्रह हमारे मन पर उस सत्य की एक टूटी-फूटी और विकृत छाया है जिसके अनुसार हमारे अन्दर एक सदात्मा है जो सबका स्वामी है और जिसके लिए तथा जिसके आदेश से ही प्रकृति अपने कर्म में लगी रहती है। इसी प्रकार अहंकार की अपनी स्वाधीन इच्छा की धारणा भी उस सत्य का एक विकृत और स्थानभ्रष्ट अनुपयुक्त भाव है जिसके अनुसार हमारे अन्दर एक स्वाधीन आत्मा है और प्रकृति की इच्छा उसी की इच्छा का परिवर्तित (modified) और आंशिक प्रतिबिम्ब है, परिवर्तित और आंशिक इसलिए कि यह इच्छा क्षण-प्रतिक्षण परिवर्तित होनेवाले काल में रहती और सतत् नये-नये ऐसे रूप धारण कर के काम करती है जो अपने पूर्वरूपों को बहुत कुछ भूले रहते हैं और स्वयं अपने ही परिणामों और लक्ष्यों को पूरा-पूरा नहीं जानते। परन्तु अन्दर की संकल्पशक्ति क्षण-क्षण परिवर्तित होनेवाले काल के परे है, वह इन सबको जानती है, और हम कह सकते हैं कि, प्रकृति का जो कर्म हमारे अन्दर होता है वह, इसी बात का प्रयास है कि अंतःस्थित संकल्प और ज्ञान के द्वारा अतिमानस-प्रकाश में जो कुछ पहले से देखा जा चुका है उसी को, प्राकृत और अहंभावापन्न अज्ञान की बड़ी कठिन अवस्थाओं में से होकर, कार्य-रूप में परिणत किया जाए।
यहाँ चर्चा यह है कि हमारा स्वतंत्र इच्छा-शक्ति का जो भान है वह एकदम गलत तो नहीं है क्योंकि हमारे भीतर एक ऐसा तत्त्व है जो पूर्णतः स्वतंत्र है और वह है हमारी अन्तरात्मा, हमारा आत्म-रूप। प्रकृति इसी के संकल्प को साधित करती है। इसलिए स्वतंत्र इच्छा का भान अपने-आप में सही है, परंतु आत्मा की बजाय उसे अहं के लिए मान बैठना गलत है। स्वतंत्रता हमारे सच्चे आत्म-रूप को है और इसी के संकल्प को प्रकृति साधित करती है। उदाहरण के लिये यदि हमने एक विशाल नाटक करने का विचार किया और उसकी मोटी-मोटी रूपरेखा बनाई, फिर विस्तार से उसका कथानक लिखा और फिर उसके अनुसार अलग-अलग पात्रों का चयन करके उन्हें उनकी भूमिकाएँ सौंपी और उसका संचालन प्रारम्भ किया। नाटक के संचालन में सभी पात्र अपनी-अपनी भूमिका अदा करते हैं। अब इसमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी पात्रों को एक-दूसरे की भूमिका का और सम्पूर्ण नाटक की विषय-वस्तु का पता हो अथवा वे उन सब चीजों को अपनी भूमिका में रहते समय याद ही रखें। नाटक खेलते समय हर पात्र का अपनी-अपनी भूमिका से तादात्म्य है। क्योंकि यदि यह तादात्म्य न हो तो इस प्रकृति को रूपांतरित नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति एक अमुक भूमिका से तदात्म नहीं होगा तो आत्मा की शक्ति से उसे रूपांतरित कैसे कर सकेगा। इसलिये यह तादात्म्य आवश्यक हो जाता है। यदि हम अपनी भूमिका में सच्चे रूप से तदात्म नहीं हैं तो फिर हम नाटक में अपनी भूमिका को सच्चे रूप से नहीं निभा सकते।
तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नाटक तो हमारा बनाया हुआ ही खेला जा रहा है। हम ही इसके रचयिता और अभिनेता हैं। पर चूंकि हमने अपनी भूमिका से अपने को तदात्म कर लिया है इसलिये हमारे द्वारा ही रचे गये इस नाटक की विषय-वस्तु को हम भूल गये हैं। और ऐसा इसलिये क्योंकि यदि हम इससे तदात्म न हों तो इस प्रकार का नाटक चल नहीं सकता, रूपांतर साधित नहीं हो सकता। यह एक देखने का तरीका है। अतः गीता अलग-अलग बातें सामने लाकर हमें सिखा रही है कि 'कर्मण्येवाधिकारस्ते....' से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वास्तव में हम स्वयं कोई कर्म कर रहे हैं। क्योंकि फिर आगे वह कहती है कि 'निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्' अर्थात् यह सब तो पहले ही हो चुका है तू, तो केवल निमित्त मात्र बन। ये सब कार्य तो होने ही हैं। क्योंकि सर्वत्र केवल मैं ही हूँ और मैं तेरी आत्मा हूँ और तुझ से एक हूँ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में मेरे संकल्प के अलावा और कुछ नहीं होता। मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही देश, मैं ही धान्य, मैं ही सम्पत्ति हूँ। यह भगवान् ने आगे नौवें अध्याय में बता दिया है। दिव्य गुरु अर्जुन को केवल इसी ओर उत्तरोत्तर विकसित कर रहे हैं।
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।। २८ ।।
२८. किन्तु हे महाबाहो अर्जुन! गुणों के विभाग और कर्मों के विभाग के तत्त्व को जाननेवाला मनुष्य, गुण परस्पर में एक-दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया किया करते हैं, ऐसा जानकर आसक्ति कर के उनके जाल में नहीं फँसता ।
....हमारी प्रगति में एक समय अवश्य ही ऐसा आयेगा जब हम अपनी आँखों को अपनी सत्ता के वास्तविक सत्य को देखने के लिए खोलने को तैयार होंगे और तब अहंभावापन्न स्वतंत्र इच्छा का भ्रम अवश्य दूर हो जाएगा... परन्तु स्वतंत्र इच्छा का त्याग किसी रूप में अपनी वास्तविक आत्मा का आभास पाये बिना, केवल भाग्यवाद को मानकर या प्रकृति की नियति को मानकर ही नहीं होना चाहिए; क्योंकि उस स्थिति में भी एकमात्र अहंकार को ही सच्ची आत्मा मानते रहेंगे और, चूँकि अहंकार सदा ही प्रकृति का उपकरण होता है, अतः हम फिर भी अहं के द्वारा ही क्रिया करते रहेंगे और हमारी इच्छा उसका यंत्र होती है, और इस प्रकार सच्ची आत्मा का विचार हमारे अंदर कोई वास्तविक परिवर्तन साधित नहीं करता, केवल हमारे बौद्धिक भाव में कुछ फेर-बदल कर देता है। तब हमने अपनी अहमात्मक सत्ता और कर्म के प्रकृति द्वारा नियंत्रित होने का व्यावहारिक सत्य तो स्वीकार कर लिया होगा, अपनी अधीनता को भी देख लिया होगा, किन्तु हमारे अन्दर जो अजन्मा आत्मा है, जो गुणों के कर्म से परे है, उसे हम न देख पाए होंगे, यह न देख पाए होंगे कि हमारी मुक्ति का द्वार कहाँ है। प्रकृति और अहंकार ही हमारी सत्ता का सर्वस्व नहीं हैं, मुक्त पुरुष भी है।... इस पुरुष की दिव्य सत्ता और स्वभाव को जानना, उसके अनुकूल होना और उसमें निवास करना ही अहंकार और उसके कर्म से निवृत्त होने का हेतु है। इससे मनुष्य गुणों की निम्न प्रकृति से ऊपर उठकर उच्चतर दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है।
प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत् ।। २९।।
२९. जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के द्वारा मूढ़ बना दिये गये हैं और गुणों की क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं, ऐसे अपूर्ण ज्ञानी मनुष्यों के मनोभाव को पूर्ण ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे।
...'अपनी' इच्छा, 'अपने' कर्म का यह विचार सर्वथा निरर्थक या निरुपयोगी नहीं है; क्योंकि प्रकृति के अन्दर प्रत्येक चीज को एक सार्थकता और उपयोगिता है। यह हमारी सचेतन सत्ता की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे अन्दर जो प्रकृति है वह अपने अंतःस्थित निगूढ़ पुरुष की उपस्थिति को अधिकाधिक जान लेती और उसके अनुकूल होती जाती है और इस ज्ञान-वृद्धि के द्वारा कर्म की एक महत्तर संभावना की ओर उद्घाटित होती है; इस अहंभाव और व्यक्तिगत इच्छा की सहायता से ही वह अपने-आपको अपनी उच्चतर संभावनाओं की ओर उठाती है, तामसी प्रकृति की निरी या फिर अधिक प्रबल निश्चेष्टता से निकलकर राजसी प्रकृति के आवेग और संघर्ष को प्राप्त होती है और फिर राजसी प्रकृति के आवेग और संघर्ष से निकलकर सात्त्विक प्रकृति के महत्तर प्रकाश, सुख और पवित्रता को प्राप्त होती है। प्राकृत मनुष्य द्वारा स्वयं के ऊपर जो आंशिक आत्मप्रभुत्व प्राप्त किया गया है वह उसकी प्रकृति की उच्चतर संभावनाओं द्वारा निम्नतर संभावनाओं पर प्राप्त किया गया प्रभुत्व है, और ऐसा उसके अन्दर तब होता है जब वह निम्नतर गुण पर संघर्ष कर के प्रभुता पाने के लिए, उसे अपने अधिकार में करने के लिए उच्चतर गुण के साथ अपने-आपको जोड़ लेता है। स्वाधीन इच्छा का बोध चाहे भ्रम हो या न हो, पर है प्रकृति के कर्म का एक आवश्यक यंत्र। मनुष्य के लिए उसके प्रगति-काल में यह आवश्यक होता है, तथा उच्चतर सत्य ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होने के पूर्व ही उसे खो देना उसके लिए अत्यंत घातक होगा... (इसीलिए गीता आदेश करती है) "...जो इन गुणों के द्वारा विमूढ़ हो जाता है...उसके मनोभाव को पूर्ण ज्ञानी विचलित न करे।"
यह एक अत्यंत गहन और सुन्दर चीज है। जैसा विशद वर्णन इसका श्रीअरविन्द ने अपने 'सावित्री' ग्रंथ में किया है वैसे वर्णन की गीता की टीका में हम उनसे अपेक्षा नहीं रख सकते। सूक्ष्म रूप में, सारे ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति में हम देखते हैं कि अवचेतन से लेकर अचेतन और निश्चेतन तक के निचले स्तरों में जो अभिव्यक्ति हुई है वह परमात्मा के गुणों से अत्यंत विपरीत चीज है। वास्तव में वह अभिव्यक्ति क्या है या कैसी है यह तो हम नहीं जानते पर मनुष्य को ऐसी प्रतीत होती है।
मनुष्यों को जब ज्ञान होता है तब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा उस निश्चेतन से अवचेतन, अवचेतन से चेतन और फिर अतिचेतन की ओर ऊपर उठते हैं। वर्तमान सृष्टि में यही प्रक्रिया गोचर होती है। यह प्रक्रिया कैसे होती है मोटे तौर पर यदि हम इसे समझें तो हम देखेंगे कि अधिकांश समय तो निश्चेतन से जड़-भौतिक तक के विकास में ही लग जाता है। जड़-तत्त्व भी एक बहुत ही लम्बे समय के बाद उत्पन्न होता है। विज्ञान इसका विकास अपने अलग ढंग से बताता है। जड़-तत्त्व के उत्पन्न होने के बाद उसमें जीवन का अभ्युदय होने में भी अरबों वर्ष लग जाते हैं। आरम्भ में अमीबा जैसे जीवाणुओं से जीवन आरंभ होता है। फिर प्रारम्भिक जीव-रूप आते हैं जो कि अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते। उसके बाद प्रकृति ऐसे जीव-रूपों को लाने का प्रयास करती है जो अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हों। अन्यथा वे जीव-रूप तो प्रकृति के थपेड़ों के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाते थे। तब हजारों-लाखों वर्षों के बाद समुद्र में जीवन का आरंभ हुआ, जिसके बाद जलथलचर जीव आए। और फिर इस कड़ी के चलते पशु आए। पशुओं में चेतना का इतना आधार तैयार नहीं होता कि वे सचेतन रूप से बोध कर सकें। साथ ही उनका जीवन सदा ही अत्यंत संदिग्ध व संकटपूर्ण होता है चूंकि एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। इसलिए यदि पशुओं को उन्हीं की वृत्ति के सहारे छोड़ दिया जाता तो वे बहुत पहले ही नष्ट हो जाते। इसलिए प्रकृति उन्हें एक सामूहिक सहजवृत्ति (instinct) प्रदान करती है। उन्हें अपनी इन्द्रियों के माध्यम से सहज रूप से पता रहता है कि क्या उनके उपयोग का है और क्या हानिकारक है। वे अपने सहजबोध से जीवनचर्या करते हैं। इस प्रकार लाखों-करोड़ों वर्ष गुजर जाने के बाद मानसिक चेतना का उदय होता है। हालाँकि पशु चेतना के अधिक निकट होने के कारण आदिम मानवों में मानसिकता का उदय अधिक नहीं था, वे सहजवृत्ति के द्वारा ही कार्य करते थे। इसके बाद धीरे-धीरे एक बड़े लंबे समय के बाद क्रमशः मानसिक चेतना का विकास हुआ जिसमें मनुष्य को इन्द्रियों के द्वारा जो कोई सूचना प्राप्त होती है मनस् उसका निरीक्षण करता है और फिर उस पर प्रतिक्रिया करता है। आरम्भ में पशु और मनुष्य दोनों को ही परिचालित करने के लिए उनमें भय और कामना लगा दी गई क्योंकि इन दो के बिना तामसिक आवरण को हिलाया नहीं जा सकता था, उसे कर्म में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता था। इसलिये कैसे मनुष्य अपनी लालसा, कामना या आकांक्षा को पूरा करेगा और कैसे अपने भय से दूर भागेगा? इसके लिए मनुष्य स्वतः ही अपनी इन्द्रियों को और अपने अर्धविकसित मन को काम में लेता है जिससे उसे थोड़ा-बहुत बोध प्राप्त होता है। परन्तु ये बोध बहुत धीरे-धीरे आते हैं और इनमें बहुत अनिश्चितता होती है, जबकि सहजवृत्ति सुनिश्चित थी। इसी कारण आरंभ में सहजवृत्ति लुप्त नहीं होती। धीरे-धीरे लाखों वर्षों के सुधार के बाद तर्क-बुद्धि विकसित हुई और सहजवृत्ति के द्वारा निर्णय कम होते गए क्योंकि यह सहजवृत्ति चेतना के एक निश्चित दायरे में ही काम करती है, उसके बाद नहीं। तर्क-बुद्धि में अधिक संभावनाएँ खुल जाती हैं और व्यक्ति अपना थोड़ा-बहुत योगदान भी देना आरंभ कर देता है। इस तर्क-बुद्धि को विकसित करना अनिवार्य ही था अन्यथा ईश्वर के रूप और उनके सत्य को कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता था? हालाँकि सहजवृत्ति में निश्चितता होती है जबकि तर्क-बुद्धि की क्रिया में त्रुटि हो सकती है, परंतु एक अधिक समृद्ध अभिव्यक्ति के लिए उसे विकसित किया गया। यदि मनुष्य को यह महसूस न हो कि वह एक पृथक् व्यक्तित्व है, तो उसमें अपने से भिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने की, उनका उपभोग करने की लालसा या आकांक्षा ही नहीं होगी और वह उनको पूरा करने की चेष्टा ही नहीं करेगा और यदि वह अपने-आप को असुरक्षित अनुभव नहीं करेगा तो वह कोई काम भी नहीं करेगा। इसलिए इस सबके लिए उसके अंदर यह अहंभाव निहित किया गया है। क्योंकि "ego is the helper, ego is the bar" अर्थात् अहं सहायक है और अहं बाधक है। व्यक्तित्व के निर्माण में अहं सहायक था। उसी के आधार पर मनुष्य के विभिन्न हिस्सों का विकास हुआ। हम देखेंगे कि जब अहंभाव होता है तो वह अपने लिये चीजों को आयत्त कर लेता है जबकि यदि यह भाव न हो तो वह ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए आरंभ में तो उसे केवल भौतिक चीजों का ही बोध होता है और सबसे पहले उसकी सहजवृत्ति अपने-आप को किसी तरह से सुरक्षित बचाए रखने की होती है। पर जैसे-जैसे उसका थोड़ा विकास होता है तो वह जान जाता है कि किस प्रकार उसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, और वह उसी प्रकार आचरण करने लगता है। इन सब अहं और अज्ञान के रूपों से होते हुए भी प्रकृति उसे आगे की ओर लिये जा रही होती है और अज्ञान के पदों को कम करती जाती है और थोड़ा-थोड़ा करके प्रकाश फैलाती जाती है। इस प्रकार प्रकृति बुद्धि का विकास करके अपने ऊपर और अंध वृत्तियों के ऊपर अंकुश लगाती जाती है। पशु ऐसा नहीं कर सकता, उसे तो अपनी सहजवृत्ति के अनुसार ही चलना पड़ता है। मनुष्य को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वह चीजों में फेरबदल कर सकता है। और जब सात्त्विक प्रकृति विकसित होती है तब व्यक्ति उचित-अनुचित का निर्णय करने में सक्षम होता है। वह सहजवृत्तियों को, भय आदि को अनदेखा कर सकता है। तब प्रकृति में अधिक लचीलापन आ जाता है और वह एक अधिक विशाल स्तर की चीज व्यक्ति के साथ कर सकती है। इस तरह का क्रमविकास हमारा चलता आ रहा है।
श्रीअरविन्द का कहना है कि गीता यह कह रही है कि हमारा अहं बोध, स्वतंत्र रूप से बुद्धि के माध्यम से सही-गलत का निर्णय करने का हमारा बोध प्रकृति का एक शक्तिशाली यंत्र है जिसके द्वारा वह दिनोंदिन अधिक चेतन होती जाती है, और तब मनुष्य अधिकाधिक सचेतन रूप से क्रिया करने लगता है और सचेतन होकर अपनी निचले स्तर की चीजों को सुधारता है। कौन ऐसा मनुष्य है जो अपनी पुरानी चीजों के प्रति सचेतन होकर उनमें सुधार नहीं कर लेता। इस तरीके से हमारे अंदर बुद्धि के अधिकाधिक विकास के साथ ही प्रकृति अधिकाधिक कुशल होती जाती है। जिस व्यक्ति को अध्यात्म ज्ञान आ गया, जिसने आत्मा का ज्ञान कर लिया, जिसने यह जान लिया कि 'सारे कर्म तो प्रकृति करती है, मैं तो इससे ऊपर हूँ', तब प्रकृति उसे इस स्तर पर ले आती है और अन्त में वह यह समझा देती है कि इस सारी प्रक्रिया से वह व्यक्ति का उत्थान कर रही थी। वास्तव में मनुष्य के अन्दर जो चीज है वह केवल इस मानसिक प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। भगवान् की परा प्रकृति है, जिसके अंदर आध्यात्मिक जगत् हैं। इसलिये व्यक्ति इन सब निम्न स्तरों से ऊपर उठ सकता है, वह इस सब से बँधा हुआ नहीं है, कोई कार्य-कारण नहीं है। हम प्रकृति के सारे नियम खोजते हैं, बुद्धि के द्वारा तुलना करते हैं, वस्तुओं तथा विभिन्न नियमों में भेद करते हैं। और फिर एक दिन हमें समझ में आता है कि ये सब बाध्यकारी नहीं हैं। वास्तव में प्रकृति तो हमारा ही दूसरा रूप है, हम स्वयं पुरुषोत्तम हैं, हमारे संकल्प मात्र से सारा ब्रह्माण्ड चलता है। यह एक बड़ी विचित्र बात है। और प्रकृति हमें उस स्तर तक ले जाएगी क्योंकि प्रकृति का तो कार्य ही यही है कि आत्म-सचेतन होकर अपनी पूर्ण चेतना में हमें पुनः ले जाना। जब हम यह जान जाते हैं कि सारे काम भगवान् की प्रकृति ही करती है और हम चाहे जो कर सकते हैं, और इस बात को हम उस मनुष्य को समझाने का प्रयास करें जो इस स्तर पर नहीं है जहाँ प्रकृति उसे गुणों के द्वारा ऊपर उठा रही है, तो वह असमंजस में पड़ जायेगा और ऐसे में वह न तो अपना कर्म कर पायेगा और न ही हमारी बताई बात का निर्वहन कर पाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को विचलित करके उसके संतुलन को भंग नहीं करना चाहिये क्योंकि उसे तो अपने अहं के कारण यही दिखाई देता है कि कर्मों का कर्ता वह स्वयं है, और उसी की प्रकृति काम कर रही है। सारे संसार में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। बड़ा विरला ही कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसे बोध हो कि गुण आदि की क्रिया तो अपनी जगह है परन्तु वह चाहे जो कर सकता है। ऐसी बात तो कदाचित् ही किसी के समझ में आती है।
इसलिये गीता यह कहती है कि पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को अपूर्ण ज्ञानी मनुष्य के संतुलन को भंग नहीं करना चाहिये। जब प्रकृति एक सीमा तक विकसित हो जाएगी तब वह ऐसा प्रकट कर देगी कि व्यक्ति यह निम्न व्यक्तित्व नहीं है। वह तो पुरुषोत्तम है, परमात्मा है। और प्रकृति उसे ऊपर उठाती है। तब फिर आध्यात्मिक प्रकृति कार्य करने लगती है। भगवान् की दिव्य पराप्रकृति ही है जो व्यक्ति की साधना कराती है। साधना कोई व्यक्तिगत प्रयत्न से नहीं होती। परन्तु यदि किसी व्यक्ति के मन में उत्साह है और वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, कभी ध्यान करता है, कभी किसी तरीके का अभ्यास करता है, कभी किसी अन्य के कहे अनुसार अभ्यास करने लगता है जैसे कि श्री रामकृष्ण जी करते थे, तो ऐसा व्यक्ति जल्दी ही आध्यात्मिकता में आगे बढ़ जाता है और जो व्यक्ति कुछ नहीं करता वह ज्यों का त्यों ही रह जाता है। अब इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बैठाया जाए? इसका कारण है कि यदि व्यक्ति वास्तव में सच्चा है, अपने उद्देश्य के प्रति कृतसंकल्प है और परमात्मा को पाना चाहता है तो उसे पाने के लिए वह सारे हथकंडे तो प्रयोग में लाएगा ही कि कौनसे तीर्थ में चला जाए, कौनसी साधना करे, कौनसी पुस्तक पढ़े, आदि-आदि। ये सब तो व्यक्ति की सच्चाई की निशानियाँ हैं। परंतु जो परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वे उन कार्यों को करने के कारण नहीं अपितु उनके बावजूद केवल उस सच्चाई के कारण उसे प्राप्त होते हैं जिसके कारण ये कर्म उत्पन्न होते हैं। परंतु यदि सच्चाई और तीव्रता के साथ-ही-साथ व्यक्ति इन सूत्रों में नहीं बँधता तो कार्य और भी अधिक शीघ्रता से हो सकता था। यह बात व्यक्ति को सहज ही समझाई नहीं जा सकती। तभी तो श्रीअरविन्द कहते हैं कि एक समय आता है जब साधना में हमें पता होता है कि हमारी साधना इतने प्रयत्नों के कारण नहीं बल्कि उनके बावजूद भी हो गई, क्योंकि परमात्मा कोई बाहरी अभ्यासों, ध्यान आदि करने से पकड़ में नहीं आ जाते। वे तो आपकी सच्चाई देखते हैं, और चूंकि आप में सच्चाई है इसीलिए आप ध्यान आदि करते हैं। आप में यह तीव्र उत्कंठग होती है कि किसी तरीके से भी मुझे भगवान् मिल जाएँ। यही सच्चाई और तीव्रता आपको परमात्मा की ओर ले जाती है। यदि ऐसी सच्चाई हो तो ध्यान ही क्यों, अन्य कोई भी चीज प्रभावी हो जाएगी। जो भी योग पद्धति व्यक्ति अपनाएगा वही प्रभावी बन जाएगी, क्योंकि उसके मूल में सच्चाई होगी। वहीं यदि कोई व्यक्ति इस नीयत से गहन ध्यान आदि भी करने लगे कि उसके द्वारा उसे कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ऐसे मनोभाव में उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसकी बजाय हो सकता है कि वह किसी गलत चीज के चंगुल में पड़ जाए। इसलिए, गीता में भगवान् ने कहा कि गुणों की यह क्रिया अनुपयोगी नहीं है। परन्तु यह ऐसी चीज भी नहीं है जिससे व्यक्ति बँधा रहे, यह ऐसी चीज है जिससे ऊपर उठा जाना चाहिये।
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।। ३०।।
३०. अपनी चेतना (चित्त) को आत्मा के साथ युक्त कर के समस्त कमाँ को मुझमें अर्पण कर के व्यक्तिगत आशा और अहंकार (मैं एवं मेरेपन) के भाव को छोड़ कर अपने आत्मा के ज्वर से मुक्त होकर युद्ध कर।
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ।। 31 ।।
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ।। 3211
३१-३२. जो श्रद्धायुक्त रहते हुए और दोष-दृष्टि से रहित हो मेरी इस शिक्षा का सर्वदा अनुष्ठान करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो दोष देखते हुए मेरी इस शिक्षा का अनुसरण नहीं करते उन्हें तू मंदबुद्धि (अज्ञ), संपूर्ण ज्ञानों में विभ्रांत, और उनका नष्ट होना नियत जान।
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।। ३३ ।।
३३. ज्ञानवान् व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, समस्त प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, हठपूर्वक दमन करने से क्या लाभ होगा?
अपनी चेतना (चित्त) को आत्मा के साथ युक्त कर के समस्त कमाँ को मुझमें अर्पण कर के व्यक्तिगत आशा और अहंकार (मैं एवं मेरेपन) के भाव को छोड़ कर अपने आत्मा के ज्वर से मुक्त होकर युद्ध कर। इस बात में सब कुछ आ गया। आत्मा का ज्वर क्या है? मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा विचार, मेरी भावना, मेरी साधना, मेरी भक्ति और न जाने क्या क्या। अगर आपकी चेतना आत्मा के साथ युक्त नहीं है तो समस्त कर्म कभी अर्पण नहीं हो सकते। क्योंकि आपकी बाहरी प्रकृति कभी कुछ अर्पण नहीं करना चाहती। यदि वह अर्पण करेगी भी तो यह सोच कर कि अर्पण करने से कुछ लाभ हो जायेगा। उदाहरण के लिए व्यक्ति भगवान् को यह सोच कर प्रसाद चढ़ाता है कि इसके बदले में वे उसका कुछ लाभ कर देंगे। इसके अतिरिक्त तो बाहरी प्रकृति का कोई और हेतु ही नहीं होता। इसलिए भगवान् कह रहे हैं कि अपनी चेतना (चित्त) को आत्मा के साथ युक्त कर के समस्त कमाँ को मुझमें अर्पण कर के व्यक्तिगत आशा और अहंकार (मैं एवं मेरेपन) के भाव को छोड़ कर अपने आत्मा के ज्वर से मुक्त होकर युद्ध कर। युद्ध क्या है, सारा जीवन ही तो कुरुक्षेत्र है इसलिए अपने अहम् और अपनी आसुरी वृत्तियों के विरुद्ध और देवत्व स्थापित करने के लिए युद्ध कर - मैं और मेरेपन के भाव को छोड़कर मुझसे जुड़कर सारा जीवन मुझे समर्पित कर दे जिससे कि मैं तेरे संपूर्ण जीवन को अपना लूँगा, उस पर अधिकार कर लूंगा और तुझे मुक्त कर दूँगा। यह जीवन का एक अटल सत्य है। इसकी उपेक्षा कर हम जीवन में कभी किसी अच्छी चीज की आशा कर ही नहीं सकते। अन्यथा तो संपूर्ण जीवन ही दुःख-दर्द से भरा है। इसके बाद, जो श्रद्धायुक्त रहते हुए और दोष-दृष्टि से रहित हो मेरी इस शिक्षा का सर्वदा अनुष्ठान करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो दोष देखते हुए मेरी इस शिक्षा का अनुसरण नहीं करते उन्हें तू मंदबुद्धि (अज्ञ), संपूर्ण ज्ञानों में विभ्रांत, और उनका नष्ट होना नियत जान। जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त होकर भगवान् की शिक्षा का पालन करते हैं, उसके संपादन का प्रयत्न करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। इसे वे कितना कर पाते हैं या उनमें कितनी योग्यता है, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि प्रयत्न करने का अर्थ है कि उनकी नीयत साफ है और अंदर विश्वास भी है, और इसलिए वे मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो दोष देखते हुए मेरी इस शिक्षा का अनुसरण नहीं करते उन्हें तू मंदबुद्धि (अज्ञ), संपूर्ण ज्ञानों में विघ्रांत, और उनका नष्ट होना नियत जान। ऐसे मनुष्य नष्ट होंगे ही क्योंकि नष्ट होने के अतिरिक्त तो उनकी और कोई नियति ही नहीं है। जब व्यक्ति की आत्मा, जिसके लिए यह शरीर बना है और वह ही सब चीजों को सहारा दे रही है, उसकी तो उसे कोई परवाह ही नहीं है तब तो शरीर संकट में आयेगा ही, जैसे एक घोड़ा जो अपने मालिक की बात नहीं मानता या ध्यान नहीं रखता उसका संकट की स्थिति में आना निश्चित ही है।
...यदि हम इस वचन को जैसा यह दिखता है उसी स्वरूप में ले लें तो प्रतीत होगा मानो प्रकृति की सर्वशक्तिमत्ता का पुरुष पर असम्भव रूप से पूर्ण आधिपत्य है।... परन्तु अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी, गीता के विचार को उसके समग्र रूप में ग्रहण करना चाहिए और उसके किसी अभिकथन को, अन्य वाक्यों के साथ के संबंध से सर्वथा अलग कर के, एकांतिक रूप से सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए।
इस विषय में एक अंतर करना होगा कि प्रकृति में वह कौन-सी चीज है जो उसका सारभूत तत्त्व, उसका मूल और अनिवार्य कार्य है जिसे रोकना, दमन करना या निग्रह करना बिल्कुल हितकारी नहीं और फिर वह कौन सी चीज है जो उसके मूल स्वभाव से संबद्ध न होकर अनावश्यक हो, जो प्रकृति का विचलन, विभ्रम और विकार है जिस पर हमें अवश्य ही नियंत्रण पाना चाहिए। निग्रह और संयम (संयम अर्थात् मर्यादित प्रयोग और उचित मार्गदर्शन) में भी भेद बताया गया है। इनमें से पहला, निग्रह, प्रकृति पर अपने संकल्प का तीक्ष्ण बल प्रयोग या हिंसा है जिससे अंततः सत्ता की स्वाभाविक शक्तियाँ अवसाद को प्राप्त होती हैं, आत्मानमवसादयेत्; और दूसरा, संयम, उच्चतर सत्ता का निम्नतर सत्ता को संयमित करना है जिससे जीव की स्वाभाविक शक्तियों को अपना स्वभावनियत कर्म और उसे करने का परम कौशल प्राप्त होता है, योगः कर्मसु कौशलम्।
vis, ii. 50
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ।। ३४।।
३४. प्रत्येक इन्द्रिय के विषय में राग और द्वेष घात लगाये बैठे हैं। उनके वशीभूत न हो क्योंकि वे दोनों आत्मा की यात्रा या पथ में उसके शत्रु (या लुटेरे) हैं।
यहाँ समझने की बात यह है कि किस प्रकार राग और द्वेष आत्मा के शत्रु और लुटेरे होते हैं और आत्मा को अपने पथ से विचलित कर देते हैं। इसे समझ लेना आवश्यक है।
इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। भगवान् धरती पर अभिव्यक्त हो रहे हैं। यह एक प्रकार की पहेली है या कह सकते हैं कि हम जगदम्बा के लिखे हुए नाटक का मंचन कर रहे हैं। जिसके द्वारा भगवान् के चरित्र, उनके विशेष गुण और शक्तियाँ आदि अभिव्यक्त हो सकें। इसमें हम सबको अपनी-अपनी भूमिका निभानी है। जिसमें कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना है और कुछ चीजों को अस्वीकार करना है। क्योंकि ऐसा करना नाटक का ही हिस्सा है। जैसे कि किसी स्थान पर पहुँचने के लिए हम अमुक सड़क लेते हैं और दूसरी को छोड़ देते हैं, इसमें कोई राग-द्वेष का प्रश्न नहीं है। और यदि हमने सड़क से ही राग-द्वेष कर लिया तो जब उसे उपयोग में लाने का समय होगा तब तो कठिनाई खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार जब तक हमारी चेतना का विकास नहीं हो जाता और जब तक वह इस स्तर पर नहीं पहुँच जाती कि हम आत्मा के रास्ते पर सहज रूप से चल सकें तब तक प्रकृति हमसे दुःख और प्रसन्नता, राग और द्वेष आदि के द्वारा कार्य करवाती रहती है। परन्तु राग और द्वेष के आधार पर किया गया व्यवहार एक बार यदि सही हो भी जाता है तो पचास बार गलत होता है। क्योंकि यदि हमने किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि के विषय में कोई पूर्वधारणा जमा रखी है तो हम उससे सहज रूप से नहीं मिल पाएँगे, सहज रूप से उसके साथ व्यवहार नहीं कर पाएँगे और केवल अपनी पूर्वधारणा के दृष्टिकोण से ही उसे देखेंगे, और नाटक में अपना भाग सही रूप से अदा नहीं कर पाएँगे। जैसे कि नाटक के एक दृश्य में हमें एक व्यक्ति से शत्रुता का व्यवहार करना है और दूसरे दृश्य में उसी व्यक्ति से प्रेम करना है तो यदि हम पूवाग्रहों से ग्रसित हैं तो हम अपनी भूमिका भली प्रकार नहीं निभा पाएँगे।
इसलिए गलत-सही या राग-द्वेष के दृष्टिकोण के आधार पर लोगों से व्यवहार करना गलत है। क्या श्रेष्ठ है, और क्या नहीं इसी आधार पर लोगों से व्यवहार करना होगा। इसीलिए भगवान् ने गीता में अर्जुन को कहा कि 'यदि तू इस दृष्टिकोण से युद्ध करेगा कि ये लोग गलत हैं और इन्होंने तेरे साथ अन्याय किया है तो तू पाप को प्राप्त होगा और यदि इस दृष्टिकोण से युद्ध करता है क्योंकि मैं तुझे कह रहा हूँ तो सारी सृष्टि का संहार करने पर भी तू पाप का भागीदार नहीं होगा। क्योंकि ऐसा करने में तू गलत नहीं होगा।' क्योंकि ऐसा करने में हम तो नाटक के कथानक का ही अनुसरण कर रहे होते हैं। और यदि हम अपने साथी अभिनेताओं के साथ राग-द्वेष, अच्छे-बुरे के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह नाटक कभी भी भली प्रकार से नहीं किया जा सकता और अधिकांश दृश्यों में हम विचलित हो जाएँगे। इसी प्रकार राग-द्वेष से ग्रसित होकर व्यवहार करने के कारण ही धरती पर सारी गड़बड़ी पैदा होती है। लम्बे समय तक स्वयं को संस्कारित करते हुए जब हम सीखते हैं तब जाकर हमारे समक्ष थोड़े से सत्य का निरूपण होता है, परन्तु थोड़ा-सा हम सीखते हैं तो अगले दृश्य में फिर गड़बड़ कर देते हैं। और इस प्रकार के उतार-चढ़ावों से गुजरते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस राग-द्वेष के पूरे प्रकरण को हम इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसे समझने के अन्य बहुत से तरीके हो सकते हैं।
---------------------
* निग्रह और आत्मसंयम में अंतर यह है कि एक कहता है "मैं कामना करना तो नहीं बन्द कर सकता पर मैं अपनी कामना को तूस नहीं करूँगा", जबकि दूसरा कहता है कि "मैं कामना और साथ ही कामना की तृप्ति दोनों को ही अस्वीकार करता हूँ।"
वास्तव में तो इसके पीछे के सत्य को उस गहरे दृष्टिकोण से देखना होगा जहाँ कि उसका विधान निहित है। इसमें राग-द्वेष करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जिस प्रकार पहेली के सभी टुकड़ों का अपना महत्त्व होता है उसी प्रकार धरती पर कोई भी चीज गलत या सही नहीं है, किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता, सभी का अपना-अपना महत्त्व है। बात बस यह है कि पहेली के टुकड़ों की ही तरह चीजों का भी अपना उचित स्थान है, और जब वे अपने उचित स्थान पर हों तो ठीक हैं और यदि नहीं, तो नहीं हैं। इनमें से किसी भी रूपक के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं।
प्रत्येक क्षण मनुष्य को सहज और तटस्थ बने रहना चाहिए, और स्वतंत्र रूप से भगवान् को ही उसके अंदर चयन करने देना चाहिये। चुनाव तो करना ही होगा। जैसे कि रास्ते में जाते समय हम यदि दाएँ मुड़ गये, तो बाँया मोड़ बुरा थोड़े ही हो गया। यदि हमें कोई कहे कि बाँया मोड़ बुरा है, तब फिर तो कहीं पहुँचा ही नहीं जा सकेगा। इसी प्रकार यदि हम किसी जाति के आधार पर संकुचित दृष्टिकोण अपना कर उसके मापदंड से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम जीवन में अत्यंत अमूल्य व्यक्तियों से मिलने का सुअवसर ही खो बैठेंगे। इसमें केन्द्रीय बात यह है कि जब तक हम अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहेंगे तब तक हम सही व्यवहार तथा प्रतिक्रिया नहीं कर पाएँगे।
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।। ३५।।
३५. भली प्रकार अनुष्ठित किये गये दूसरे के धर्म की तुलना में दोषपूर्ण होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ होता है; अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ होता है, परधर्म का अनुसरण करना विनाशकारी होता है।
इस स्वधर्म का वास्तविक अर्थ जानने के लिए हमें तब तक ठहरना होगा जब तक गीता के बाद के अध्यायों में किए गए पुरुष, प्रकृति और गुणों के विस्तृत विवेचन तक न पहुँच जाएँ, परन्तु निश्चय ही इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसे हम प्रकृति कहते हैं उसकी जो कोई भी प्रेरणा हो, चाहे वह अशुभ ही क्यों न हो, उसका पालन करना होगा।... गीता कहती है, पापकर्म से निवृत्ति अथवा उसका त्याग मुक्ति की पहली शर्त है और सर्वत्र गीता आत्मप्रभुत्व और आत्मसंयम का तथा मन, इन्द्रियों और सम्पूर्ण निम्न सत्ता के संयम का उपदेश करती है।
इसमें सबसे पहले तो श्रीअरविन्द यह समझाते हैं कि इस बात के क्या-क्या गलत अर्थ लगाए जा सकते हैं। जैसे कि, अलग-अलग धर्म के व्यक्ति अपने-अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएँगे, जबकि इस उक्ति का उस धर्म के सामान्य अर्थ से कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ मत-सम्प्रदायों के बारे में बात नहीं हो रही है। दूसरा गलत अर्थ लगाने का तरीका है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर (जो कि स्वयं भी आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़े हुए व्यक्ति थे) ने दिलीप कुमार रॉय को कहा कि 'दिलीप तुम और मैं योगी नहीं हैं, हम तो अपनी प्रकृति से कलाकार हैं। इसलिए योग करना तुम्हारा काम नहीं है।* जब दिलीप कुमार रॉय ने इसके बारे में श्रीअरविन्द को लिखा तो श्रीअरविन्द ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कुछ इस प्रकार कहा कि "ये सब बातें निरर्थक हैं। और इन सब संदेह के अंतरालों को व्यक्ति को सहन करना ही होगा और तब तक डटे रहना होगा जब तक उषा नहीं आ जाती।" इसमें समझने की बात यह है कि अधिकांश लोग अपने धर्म का अर्थ उनकी अपनी प्रकृति के गठन के अनुसार लगाते हुए कहते हैं कि 'हम तो व्यापारी हैं, यह ये हैं, हम वो हैं और हमारी प्रकृति तो ऐसी ही बनी हुई है, हमने तो सदा ही इसी तरीके से कर्म किया है और हमारा धर्म तो यही है कि हम इस प्रकार से चलें', आदि-आदि। परन्तु इन सब बातों का गीता के धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये तो दुराग्रह हैं, मूर्खताएँ हैं, एक प्रकार की बेड़ियाँ हैं।
गीता जिस धर्म की बात कर रही है वह न तो कोई मत-सम्प्रदाय है और न ही यह कि आपकी प्रकृति इसी प्रकार की रही है कि आप किसी समुदाय में पैदा हुए हैं या किसी परिवार में पैदा हुए हैं इसलिए उसके नियम या व्यवहार आदि का आँख मूँदकर अनुसरण करते जाएँ। गीता यहाँ इस प्रकार की बात नहीं कर रही है।
--------------
* योगी श्रीकृष्णप्रेम, पृष्ठ ३९, श्रीअरविन्द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट
स्वधर्म वास्तव में वह मार्ग है जो आपकी आत्मा अपने-आप को अभिव्यक्त करने के लिए अपनाए। इसीलिए 'स्वभाव नियत कर्म' की बात गीता में कही गई है। और इसमें व्यक्ति को अपने सतही भाव से वास्तविक और सच्चे स्वभाव में जाना होता है और फिर स्वभाव से सभी धर्मों का परित्याग करके भगवान् के मद्भाव में। इसलिए जो आपका सहज आन्तरिक स्वभाव है, और जिसकी ओर जाना आपका काम है उसमें जो आपकी मदद करता है वह आपका स्वधर्म है। आपके स्वभाव की अभिव्यक्ति होगी तो वह स्वधर्म है, अन्यथा वह स्वधर्म नहीं है। गीता में इस बात को आगे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाएगा।
प्रश्न : यहाँ जो उदाहरण दिया है, कि हम सब की नाटक में अलग-अलग भूमिकाएँ हैं, तो क्या हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हम वह भूमिका छोड़ कर दूसरे की भूमिका निभाने लगते हैं?
उत्तर : वास्तव में स्वभाव क्या है? श्रीमाताजी की अनन्त शक्तियाँ और विभूतियाँ हैं। श्रीअरविन्द का कहना है कि उन अनंत शक्तियों में से धरती पर उनकी केवल चार ही शक्तियाँ मुख्य रूप से कार्यरत हैं, अतः व्यक्ति के अन्दर जिस शक्ति की क्रिया की प्रधानता होगी व्यक्ति को उसी के अनुरूप कर्म करने में सुविधा होगी। जैसे कि व्यक्ति में महाकाली की क्रिया की प्रधानता हो पर उसे सेवा करने के लिए कह दिया जाए तो वह क्या सच्ची सेवा कर पाएगा? या फिर यदि व्यक्ति के अन्दर ज्ञान पक्ष प्रवल है और ज्ञान की पिपासा है तब सेवा कर्म वह उतनी भली प्रकार नहीं निभा पाएगा। इसे समझने के लिए चाहे हम इसे नाटक में भिन्न-भिन्न भूमिका बोल सकते हैं या फिर इन शक्तियों की भिन्न-भिन्न क्रिया के अनुसार इसे समझ सकते हैं, हालाँकि इन शक्तियों के अनुसार इसे समझना अधिक सरल है। स्वभाव के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था की गई थी। परन्तु वास्तव में तो व्यक्ति स्वभाव से बँधा हुआ नहीं है। व्यक्ति तो श्रीमाताजी से बँधा हुआ है। वह इन शक्तियों से भी बँधा हुआ नहीं है और इन शक्तियों की प्रमुखता व्यक्ति के जीवन में एक सीमा से अधिक नहीं होती। क्योंकि ये शक्तियाँ तो भगवान् की आद्याशक्ति, जो कि जगदम्बा हैं, की अभिव्यक्तियाँ हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वभाव-नियत कर्म करते-करते श्रीमाँ की ओर चलना होता है और फिर स्वभाव से ऊपर उठकर (मद्भावमागता) पुरुषोत्तम के, अथवा जगदम्बा के मद्भाव की ओर जाना होता है। उसी के लिए सारी साधनाएँ और उनके बाद 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' आदि सब बताए गए हैं। हिन्दुस्तान में यह व्यवस्था थी कि जब सारे समाज को, सारी मनुष्यजाति को परमात्मा की ओर ले जाना है, तब कौन-सा व्यक्ति कौन-सा काम करके उस ओर जा सकता है यह उसके आन्तरिक स्वभाव पर निर्भर करेगा, न कि उसकी बाहरी प्रकृति पर। एक ही परिवार में अलग-अलग स्वभाव के लोग हो सकते हैं और उन सबको एक ही प्रकार की प्रकृति से ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयत्न किया जाए तो सब अनर्थ हो जायेगा क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग-अलग होता है। और जो उस स्वभाव के अनुसार है वही 'स्वभाव नियत कर्म' है।
अर्जुन उवाच
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।
अनिच्छन्नपि वाष्र्णेय बलादिव नियोजितः ।। ३६।।
३६. अर्जुन ने कहाः हे वाष्र्णेय श्रीकृष्ण ! यदि अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने में कोई दोष नहीं है तो हमारे भीतर यह क्या है जो मनुष्य को पाप कर्म की ओर मानो बलपूर्वक प्रवृत्त करता है, यहाँ तक कि अपनी संघर्ष करती हुई इच्छा के विरुद्ध भी?
श्रीभगवान् उवाच
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम् ।। ३७।।
३७. श्रीभगवान् ने कहाः रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला यह काम" है, यह (उसका) साथी क्रोध है; यह काम सर्वभक्षी, महापापी है; इस संसार में इस काम को मानव आत्मा का शत्रु समझ ।
यहाँ पर यह वर्णन है कि कामना बहुत ही खराब है। परन्तु इसका क्या कारण है, इसे समझ लेना आवश्यक है।
यहाँ जो वर्णन है वह यह है कि कामनाओं का एक समुद्र है। व्यक्ति महसूस करता है कि कामना उसकी अपनी होती है या उसके अपने अंदर से उत्पन्न होती है। जबकि वास्तव में वह बाहर से आती है। कामना एक सतही चीज है। उदाहरण के लिए व्यक्ति के मन में खाने-पीने की या अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने की चाह उठती है। इस काम का मूल स्रोत कहाँ है, ये कामनाएँ उठती कहाँ से हैं? मनुष्य का विकृत या क्रमविकास से आया प्राण ही इन भावों के प्रति प्रत्युत्तर देता है। और वही मनुष्य की सारी सत्ता को भी आच्छादित करता है और व्यक्ति के मन व शरीर को भी प्रभावित करता है। इसकी विकृति के पीछे वेदों में वर्णित वृत्र, पणि आदि आसुरिक शक्तियाँ और प्राणिक जगत् की सत्ताएँ होती हैं। इस विकृत प्राण के द्वारा ये शक्तियाँ मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं जिससे व्यक्ति संतुष्टि और अपने क्षणिक आवेग में सुख का अनुभव करता है, जबकि वास्तव में तो व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया जाता है। इस प्रकार की इसकी प्रकृति है।
अब प्रश्न यह है कि जब व्यक्ति किसी बदमाश आदमी के कहे अनुसार कोई काम कर रहा है और उसके अनुसार चल रहा है तब वह अपने गन्तव्य स्थान तक कैसे पहुँच पाएगा? ऐसी स्थिति में वह आत्मा का कोई सच्चा काम तो कर ही नहीं सकता क्योंकि यह तो सारी बड़ी व्यवस्थित ढंग से की गई बदमाशी है। और कोई भी व्यक्ति इसे महसूस तक नहीं कर पाता क्योंकि सारे समाज में ऐसी परिपाटी बन चुकी है, सभी इसके इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि इस पर कभी कोई संदेह तक भी नहीं करता कि हमारे साथ ऐसी कोई बदमाशी या जालसाजी चल रही है। श्रीमाँ ने इस बारे में कहा कि कामनाओं का समुद्र है, जो भी बाहर से कामना आती है वह पहले अवचेतन में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से चित्त के द्वारा ऊपर उठती है और तब व्यक्ति में यह कामना सतह पर इस आवेग के रूप में उठती है कि अमुक काम कर लें, यह चीज खा लें या यहाँ-वहाँ घूम आएँ, आदि-आदि।
अब इसमें समस्या यह आती है कि कामनाओं के पीछे और भी बहुत सी चीजें होती हैं जैसे, इच्छा-शक्ति, संकल्प-शक्ति, आदि-आदि। इन चीजों में भेद कर पाना आसान नहीं होता और न ही इस स्तर पर व्यक्ति इन चीजों से सामना या मुकाबला ही कर सकता है। क्योंकि ये सारे भाव सतह पर तो कामनाओं के रूप में ही ऊपर उठते हैं और यदि व्यक्ति इनका विरोध करता रहे तो जीवित ही नहीं रह सकेगा। इस तरीके के व्यावहारिक अनुभव की बातों का सामान्यतया पुस्तकों में वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा करना आसान नहीं है। अब जटिल समस्या यह है कि कामनाओं पर काबू कैसे किया जाए, उन पर लगाम कैसे लगाई जाए।
---------------
"कामना निम्न प्रकृति की सबसे अधिक अंधकारमय और सबसे अधिक अंधकारमय बनाने वाली गति है। कामनाएँ दुर्वलता और अज्ञान की गतियाँ हैं और वे तुम्हें अपनी दुर्बलता तथा अज्ञान से बाँधे रखती हैं। लोगों की धारणा है कि उनकी कामनाएँ उनके अपने अन्दर उत्पन्न होती हैं, उन्हें लगता है कि ये या तो उनके अपने-आप में से पैदा होती हैं या उनके अपने अन्दर से उठती हैं; किन्तु यह एक मिथ्या धारणा है। कामनाएँ अंधकारमय निम्न प्रकृति के विशाल समुद्र की लहरें हैं और वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचती रहती हैं। मनुष्य कामना को अपने-आप में उत्पन्न नहीं करते, अपितु इन लहरों द्वारा आक्रांत होते हैं, जो कोई इनके लिये खुला होता है या जो सुरक्षारहित होता है वह इनकी पकड़ में आ जाता है और इनके थपेड़ों को खाता हुआ इधर-से-उधर डोलता रहता है। उसे अभिभूत कर के और उस पर अधिकार कर के कामना उसे किसी भी प्रकार का विवेक करने में असमर्थ बना देती है और उसमें ऐसी धारणा जमा देती है कि इस (कामना) को चरितार्थ करना भी उसके अपने स्वभाव का एक अंग ही है। परंतु वस्तुतः इसका मनुष्य के सच्चे स्वभाव के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। ईर्ष्या, डाह, घृणा और हिंसा आदि सभी निम्नतर आवेगों के सम्बन्ध में यही बात है। ये भी ऐसी गतियाँ हैं जो तुम्हें पकड़ लेती हैं, ऐसी लहरें हैं जो तुम पर चढ़ आती हैं और आक्रांत करती हैं; इनका सच्चे चरित्र या सच्चे स्वभाव से कोई सम्बन्ध नहीं, ये तो उन्हें विरूप बनाती हैं। ये तुम्हारा कोई नैसर्गिक या अविभाज्य अंग नहीं हैं, अपितु इर्द-गिर्द के उस अन्धकारमय समुद्र से आती हैं जिनमें निम्न प्रकृति की शक्तियाँ विचरण करती हैं। इन कामनाओं, इन आवेशों का कोई व्यक्तित्व अथवा विशिष्ट स्वरूप नहीं होता... ये इसी रूप में सभी के अन्दर अभिव्यक्त होती हैं।
इसीलिए भले ही इस पर काबू करने की या इस पर लगाम कसने की शिक्षा तो बहुत दी जाती है, परन्तु उसका अनुसरण कदाचित् ही कोई कर पाता है क्योंकि अधिकांशतः शिक्षा देने वाला और पाने वाला दोनों ही इस बात को नहीं समझते हैं। अतः यह पूरा विषय बहुत ही जटिल है।
अब प्रश्न यह है कि यह कैसे पता चले कि अमुक भाव कामना है या इच्छा-शक्ति है, या फिर आंतरिक संकल्प है, या फिर अभीप्सा का ही कोई रूप है या फिर कुछ और है। क्योंकि यदि सारी उत्प्रेरणाओं को कामना ही मान लिया जाए और सभी को कामना कह कर त्याग दिया जाए तब तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि फिर न वह कुछ खा सकेगा, न पी सकेगा और न कुछ कर सकेगा। इस समस्या को कैसे हल किया जाए। हम पहले यह चर्चा कर चुके हैं कि कामना की क्या प्रकृति है, कैसे वह बाहर से आती है, किस प्रकार वह हमारी आत्मा को आच्छादित करती है। तो क्या हमारी सत्ता में कामनाएँ ही हैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इसके पीछे क्या-क्या चीजें हैं?
एक साधक : एक तो जिसकी कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारे अन्दर कोई ऐसी चीज है जिसे किसी चीज की चाह है, और कामनाएँ इस चीज से ऊर्जा लेकर स्वयं को अभिव्यक्त करती हैं। और दूसरी बात है कि प्राणिक जगत् की सत्ताएँ होती हैं जो कि कई चीजों में संलग्न रहती हैं और अपनी संतुष्टि के लिए मनुष्यों को इस्तेमाल करती हैं और हमें लगता है कि ये हमारी अपनी कामनाएँ हैं और हम उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हैं।
प्रश्न : परन्तु प्रश्न यह है कि यदि व्यक्ति अपने-आप को अनुशासित कर आगे बढ़ना चाहे तो व्यावहारिक रूप में उसे क्या करना चाहिये?
एक साधक : शायद इसमें हम अपनी सामर्थ्य से तो बहुत ही कम कर सकते हैं। हम तो केवल श्रीमाताजी से प्रार्थना ही कर सकते हैं और उनके प्रति अपने को खोल सकते हैं। केवल वे ही हमें रास्ता दिखा सकती हैं कि सच्ची चीज क्या है और हमें उसका अनुसरण कैसे करना है।
उत्तर : गीता यहाँ जो समाधान बता रही है वह बिल्कुल व्यावहारिक और करने योग्य है। इसमें पहले तो भगवान् ने कह दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना फल की इच्छा के कर्म कर। परन्तु इसमें समस्या यह आती है कि निर्णय कैसे करें कि क्या कर्म करने का है और क्या करने का नहीं है। इस बात का समाधान करते हुए भगवान् ने कहा कि 'यज्ञ के रूप में कर्म कर।' मेरी प्रसन्नता के निमित्त कर्म कर। और यदि भगवान् की प्रसन्नता के निमित्त कर्म करेंगे तो उसमें हमारा अनुमान कि भगवान् की प्रसन्नता कौनसे काम में है, वह तो सदा ही बड़ा सापेक्ष या अनिश्चित प्रकार का होगा। क्योंकि यज्ञ पहले तामसिक, होता है, फिर राजसिक और उसके बाद सात्त्विक। व्यक्ति को इससे होकर गुजरना ही पड़ेगा। वेदों के साधनाभ्यास में तो बड़ी जबरदस्त बातें हैं जो कि देश, काल, पात्र के अनुसार हैं। व्यक्ति यदि इनका अध्ययन आदि करके इनसे जुड़ सके तो वह कुछ कर पाएगा। परन्तु इसके साथ-साथ व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन मिलना आवश्यक है। और उसके लिए व्यक्ति को अंदर से जुड़ना पड़ेगा।
हालाँकि इसके अंदर बौद्धिक ज्ञान आदि भी सर्वथा निरर्थक नहीं हैं। भले ही अपने आप में वे कितने भी सीमित क्यों न हों, पर उनकी अपनी उपयोगिता है क्योंकि ये आधार को तैयार करने का काम करते हैं। इसलिए यदि कुछ बौद्धिक आधार तैयार हो तो जब व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है तो आरम्भ में वह बुद्धि में बने हुए आधार को ही काम में लेती है और विभिन्न हिस्सों को अनुशासित करती है। फिर जब धीरे-धीरे व्यक्ति को आभास होता है कि उसकी बुद्धि भी विश्वसनीय नहीं है तब धीरे-धीरे उसे और गहरा अंतर्भास या अंतःप्रज्ञा प्राप्त होगी। परन्तु यदि व्यक्ति में कोई भी आधार तैयार नहीं है तो उसके लिए विभिन्न उत्प्रेरणाओं तथा विभिन्न क्रियाओं के बीच में भेद करना कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस आधार के बिना वह अंतर्भास नहीं आ सकता, परंतु वह और अधिक कठिन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे शास्त्र, जो कि आरोहणशील यज्ञ की चर्चा करते हैं, उपयोगी हैं। क्योंकि यह बात तो निश्चित है कि कामना को नियंत्रित करना कोई आसान चीज नहीं है। भागवत् संकल्प अधिकांशतः हमारे अंदर कामना के रूप में ही कार्यान्वित होता है। हालाँकि यह क्रिया बड़ी अपरिष्कृत या भद्दी है, परंतु सामान्यतः हम इसी क्रिया के प्रति खुले हुए होते हैं, इसलिए भागवत् संकल्प इसी प्रक्रिया के द्वारा अपना काम कर लेता है। चूंकि वह अवचेतन से होकर अपना काम करता है, इसलिये कामना आदि उससे चिपक जाते हैं, और उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। परंतु दिव्य विधान को उस दुरुपयोग का पता होता है और वह उसकी गुंजाइश रखता है। इसलिए यह ऐसी चीज नहीं है कि व्यक्ति मन में सोच ले और कर ले।
दुनिया में किसी भी महत्त्वपूर्ण चीज की स्थापना के लिये पूरी ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि व्यक्ति की सत्ता बड़ी जटिल है। इसमें बहुत तरीके के समीकरण हैं, भिन्न-भिन्न सत्ताएँ का इसमें प्रवेश है और उन सबका अपना-अपना प्रभाव होता है। हालाँकि इन सबका अपना औचित्य तो है परन्तु वर्तमान में ये अपने यथास्थान पर न होकर स्थानभ्रष्ट हैं। इसलिए उस महत्त्वपूर्ण चीज को स्थापित करने के लिए व्यक्ति को आश्रय लेना होगा परमात्मा की ओर अभीप्सा का, इच्छा-शक्ति, संकल्प आदि का, और इन सब को काम में लेकर व्यक्ति उस ओर अग्रसर होता है और तब जाकर इस विकट समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसी अन्य तरीके से यह नहीं हो सकता। किसी एक ही ऐसे सूत्र से यह नहीं हो सकता कि : कामना नहीं होनी चाहिये, या यह नहीं होना चाहिये या वह नहीं होना चाहिये। हाँ, व्यक्ति कोई व्यावहारिक परामर्श तो दे सकता है कि लालच से खाना नहीं खाना चाहिए, केवल शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही खाना चाहिए। हालाँकि कामना तो उसके पीछे भी छिप जाएगी, बस उसका भोंडापन कुछ कम दिखाई पड़ेगा। परंतु केवल समझाने से ऐसी चीजें समझ आनी मुश्किल हैं क्योंकि कामना आदि की सत्ताओं ने मनुष्य पर अपना कब्जा जमा रखा है और जब तक कोई गहरी चीज नहीं आ जाती तब तक केवल समझाने से यह नहीं हो सकता। क्योंकि जीभ के स्वाद जैसी ही अनेकानेक चीजों के प्रति अतिशय आसक्ति से ऊपर उठ पाना सहज नहीं है कि केवल समझाने pi से ही व्यक्ति उन पर विजय पा सके।
यही बात मोह के बारे में है। मोह तो अंधा होता है। अब यदि किसी को यह समझा दिया जाए कि आपको अपने दोस्त, अपने परिवार के सदस्य या किसी से भी मोह नहीं रखना चाहिए तो क्या यह व्यक्ति के वश में है कि वह मोह न रखे? इसलिए वास्तव में लाख दुःखों की एक ही दवा है और वह है श्रीमाँ की ओर मुड़ जाना और तब फिर धीरे-धीरे ये सभी व्याधियाँ अपने-आप ही झड़ जाएँगी। जैसे गंगा जी में एक बार स्नान करने से कुछ पाप झड़ जाते हैं, और यदि बार-बार स्नान करेंगे तो सब झड़ जाएँगे। इसी प्रकार श्रीमाँ की ओर चलेंगे तो रास्ते में कुछ-न-कुछ व्याधियाँ तो झड़ेंगी ही। चलने का सारा मार्ग ही तो गीता बता रही है - और वह है उत्तरोत्तर 'यज्ञ का आरोहण'। धीरे-धीरे यज्ञ भी क्रमशः ऊपर चढ़ता जाता है। और यदि हमें वास्तव में यह करना है, और मन में यह इच्छा आ जाए, उसके लिए संकल्प आ जाए तो भगवान् की सहज व्यवस्था ऐसी है कि वे हमारा मार्गदर्शन किसी पुस्तक के माध्यम से, जीवन के थपेड़ों के रूप में, किसी मित्र की अच्छी सलाह के रूप में या फिर अंततः सद्गुरु के रूप में करेंगे। इस व्यवस्था का विधान तो पहले से ही भगवान् के द्वारा किया गया है, इसलिये इसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी आवश्यक चीजों की व्यवस्था स्वयं ही हो जाएगी, बस आवश्यकता एक ही बात की है कि किसी तरह से हमारे अन्दर यह जाग्रति आ जाए कि हमारे साथ जो निम्न प्रकृति का अनाचार चल रहा है उसे हम और अधिक सहन नहीं करने वाले हैं। यदि यह संकल्प आ जाए कि भले ही अभी हम कमजोर हैं, फिर भी हम उन रास्तों का पता लगाएँगे, वे उद्योग करेंगे, वे हथियार अपनाएँगे जिससे हमें इन चीजों से छुटकारा मिले, तब फिर वह प्रभावी होता है। इसमें व्यक्ति के गठन के अनुसार समय कम या अधिक लग सकता है परन्तु यह काम होगा अवश्य, यह रुक नहीं सकता क्योंकि परमात्मा की ऐसी निर्दय व्यवस्था नहीं है कि हम वास्तव में करना चाहें और वह काम न हो।
यह केवल एक आसुरिक सुझाव है कि आखिर व्यक्ति के चाहने भर से ही क्या हो जाएगा। वास्तव में तो चाहने से ही सब कुछ होता है। प्रकृति व्यक्ति की सच्ची चाह के प्रति प्रत्युत्तर देती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हालाँकि, उसका अपना विधान है। इसमें यदि व्यक्ति यह सोचे कि उसने तो चाह कर ली है इसलिए अब तो वैसा हो ही जाना चाहिये, तो इससे काम नहीं होने वाला। जैसे कि यदि व्यक्ति यह चाह कर ले कि उसके माता-पिता उसके लिए कोई अच्छा महल बना दें, तो चूंकि यह जड़ जगत् है, इसलिए यदि वे कोई महल बनाने को तैयार भी हों तो भी उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, अपना तरीका है, जिसमें आवश्यक समय, ऊर्जा और संसाधन लगेंगे। उसे बनाने के लिए न जाने क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। वहीं यदि हम अपने अन्दर परमात्मा के मन्दिर का निर्माण करना चाहते हैं, परमात्मा से एक होना चाहते हैं तो उसमें हमें थोड़ा धीरज और विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। इसका और कोई सरल उपाय नहीं है। और यदि हमें इसमें भेद जानना है कि अमुक चीज कामना है या नहीं तो इसके लक्षण हैं। हम यह इससे परख सकते हैं कि कामना का आवेग हमको एकाएक ही पकड़ लेता है। दूसरे यदि किसी चीज के लिए कोई आवेग उठे तो उसमें हम यह प्रश्न करें कि क्या वह वस्तु हमारे लिये आवश्यक है या नहीं। इसी प्रकार भोजन की कामना भी बड़े तीव्र रूप से उठती है। उसके अनुशासन के लिए हमारी संस्कृति में संयम के अनेकों तरीके बतलाए गए हैं कि सात्त्विक भोजन करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उससे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। व्यावहारिक तौर पर तो इसी प्रकार के अंकुश और अनुशासन लागू किये जा सकते हैं।
काम-प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, उसे संयमित करने के लिए भी कई उपाय किये गए। यह कहा गया कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए यह क्रिया की जा सकती है। इसके पीछे निरंकुश भोगेच्छा की बजाय इसके साथ एक कर्तव्य बोध जोड़ दिया गया। और उसके ऊपर बड़े प्रतिबन्ध लगा दिए गए। इन सब नियमों का मूल उद्देश्य यही था कि व्यक्ति की आत्मा को साँस लेने का थोड़ा मौका मिल सके अन्यथा तो सारे दिन ही अपनी इंद्रियों की तृप्ति में, जीभ के स्वाद में, लोभ-लालच आदि में ही लगा रहेगा।
ऐसे ही आसक्ति की बात है। यदि व्यक्ति आसक्ति को रोक नहीं सके तो कम-से-कम उसके दुष्प्रभाव को यह सोच कर कम तो कर ही सकता है कि ये सब भगवान् के ही रूप हैं। इतना तो किया जा ही सकता है। जैसे यदि आपको अपने मित्र में बहुत आसक्ति है और यदि आप यह सोचो कि यह तो मेरा साँवरिया ही है और उसी से मेरी दोस्ती है तो आपका बहुत बचाव हो जाएगा। इन सारे बचाव के रास्तों के लिए ही तो धर्म में ये सब बातें बताई गई हैं। ये सभी अपूर्ण होते हुए भी हैं बड़े कारगर व्यावहारिक समाधान। सच्चा समाधान तो यही है कि व्यक्ति अपने जीवन को यज्ञमय बना दे और उत्तरोतर भगवान् की ओर आरोहण करे अन्यथा कोई भी समस्या यों हल नहीं होने वाली। सारी समस्याओं के लिए व्यक्ति को कृतसंकल्प होना होगा कि किसी भी कीमत पर वह उन सभी की सफाई करेगा। और उसके लिए इतना संकल्प हो कि जो कुछ भी उसके लिए आवश्यक हो वही वह करने के लिए तैयार रहे। ऐसा व्यक्ति अवश्य सफल होगा।
जो विकृति भीतर प्रवेश कर के शुद्धता अथवा पवित्रता में बाधा डालती है वह एक प्रकार की प्राणिक लालसा है; अतीन्द्रिय सूक्ष्म-प्राण (psychic prana) हमारी सत्ता में जो सबसे बड़ी विकृति ले आता है वह है कामना। कामना का मूल है जिस वस्तु का हम अभाव अनुभव करते हैं उसे अधिकृत करने की प्राणिक लालसा, यह है अधिकृत करने और तुष्टि प्राप्त करने के लिये हमारे सीमित प्राण की सहज प्रवृत्ति। यह अभाव के बोध को जन्म देती है, - पहले तो क्षुधा, पिपासा, काम-वासना जैसी अधिक सीधी-सादी प्राणिक लालसाओं को और फिर मन की इन सूक्ष्म-अतीन्द्रिय क्षुधाओं, पिपासाओं और कामवृत्तियों को जन्म देती है जो कि हमारी सत्ता में अधिक शीघ्रता से उत्पन्न होने वाली तथा पूरी सत्ता को व्याप्त करने वाली अधिक भीषण वेदनाएँ हैं, (कामनाजन्य) एक ऐसी क्षुधा जो अनन्त होती है, क्योंकि यह एक अनन्त सत्ता की क्षुधा होती है, यह पिपासा भी तृप्ति के द्वारा केवल कुछ समय के लिये ही शान्त हो सकती है, पर अपने स्वभाव में यह अतृप्य ही होती है।... कामना समस्त दुःख, निराशा और वेदना की मूल होती है; क्योंकि, यद्यपि इसमें विषयों के पीछे दौड़ने तथा उनसे तुष्टि प्राप्त करने का उत्तेजनात्मक हर्ष होता है, पर, क्योंकि यह सदा ही सत्ता पर तनाव डालती है, यह अपनी भागदौड़ तथा प्राप्ति में श्रम, क्षुधा और संघर्ष को साथ लिये रहती है, शीघ्र थक जाती है, परिमितता अनुभव करती है, अपनी सभी प्राप्तियों से असन्तुष्ट होकर शीघ्र ही निराश हो जाती है, अविरत दूषित उत्तेजना, क्लेश एवं अशान्ति को अनुभव करती है।
अब इसका वर्णन दे दिया कि कामनाएँ अशान्ति पैदा करती हैं। इसमें भौतिक कामनाएँ तो एक बार पूरी होने के बाद कुछ समय के लिए रुक जाती हैं। जैसे कि खाने की कितनी भी कामना क्यों न हो पर उसे तृप्त करके एक बार पेट भरने के बाद कुछ समय के लिये वह तुम्हें छोड़ देगी। परन्तु जो मनोवैज्ञानिक क्षुधाएँ-तृष्णाएँ हैं, जैसे कि संसार में ख्याति प्राप्त करने, बड़ा पद प्राप्त करने की क्षुधा, और न जाने अन्य कितनी असंख्यों क्षुधाएँ हैं, वे कभी शान्त नहीं होतीं। वे तो बढ़ती ही जाती हैं।
इसके साथ ही दूसरी आशंका यह भी बनी रहती है कि कहीं व्यक्ति आसुरिक प्रवृत्ति द्वारा अधिकृत न कर लिया जाए। उदाहरण के लिए, व्यक्ति के पास भले कितना भी धन क्यों न एकत्रित हो जाए, परन्तु उसकी लालसा कभी शान्त नहीं होती। भोजन से तो पेट भर जाता है परन्तु इससे कभी भी नहीं भर सकता। क्योंकि पैसे के पीछे बड़ी भद्दी आसुरिक शक्तियाँ हैं। यही नाम, पद, अधिकार आदि की भी बात है। व्यक्ति को कितना भी अधिकार क्यों न प्राप्त हो, फिर भी उसे और अधिक की लालसा रहती है। इसमें केवल इतना बताया गया है कि ये चीजें व्यक्ति के जीवन में बहुत अशान्ति ले आती हैं और वह और कुछ न कर के केवल अपने आवेगों को ही पूरा कर रहा होता है। और इसी के माध्यम से भागवत् इच्छा अपना थोड़ा-बहुत काम करती है और व्यक्ति की सत्ता उन्हीं स्पंदनों में चलती रहती है और उसकी दुर्गति होती रहती है। अधिकांशतः निम्न शक्तियाँ ही अपने-आप को अभिव्यक्त करती हैं, कोई अच्छी चीज तो अपने को अभिव्यक्त कर ही नहीं पाती। कोई आन्तरात्मिक चीज तो अभिव्यक्त हो ही नहीं पाती क्योंकि सामान्य व्यक्ति की प्रकृति ही इस प्रकार की होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में इस सब के संयमन की, इस सब के शमन की व्यवस्था अंतर्निहित थी। पश्चिम में इन चीजों को छूट दे दी गई और उसके दुष्परिणाम हम देख ही रहे हैं।
इसके विपरीत, व्यक्ति के मन में ज्यों ही किसी के प्रति सच्ची निष्ठा का भाव आ गया, कोई सद्भाव आ गया, तो फिर कामनाओं आदि की प्रयोजनीय हो। इसलिए इन चीजों में हमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी अपेक्षा हमें तो ये चीजें श्रीमाताजी के हाथों में सौंप देनी चाहिए। अहं को भी हम उनके हाथों में सौंप दें और जितना वे उसे काम में लेना चाहें उतना लें, हमें उससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए। वैसे ही कामनाओं के बारे में तथा अन्य सभी चीजों के बारे में है। सारी चीजों को श्रीमाताजी के प्रति समर्पित करना होगा, और समर्पण होता है प्रेम के द्वारा। प्रेम आता है कामनाओं पर नियंत्रण करने से और कामना नियंत्रित होती है प्रेम के आने से। तो यह कैसे हो? इसका हल भागवत् कृपा के हस्तक्षेप से होता है।
परंतु इसका एक ही परम समाधान है कि सभी कुछ को श्रीमाँ के प्रति समर्पित कर दिया जाए। क्योंकि बाकी सभी सूत्र या तरीके जब तक व्यक्ति साधना के मार्ग पर नहीं आता तब तक तो उपयोगी हो सकते हैं परन्तु जब व्यक्ति साधना के मार्ग पर सचेतन रूप से आ जाता है तब सब कुछ केवल श्रीमाँ के हाथ में छोड़ देना ही उचित है। इसके अतिरिक्त और कोई समाधान दिखाई नहीं देता। वास्तव में, केवल वे ही जानती हैं कि क्या त्यागना है और क्या नहीं, और साथ ही यह कि कितना त्यागना और कितना रखना है। और चूँकि हमें इस सब का पता नहीं होता इसलिये यदि हमने बड़े साधन से, बड़े यत्न से कामना को, या अन्य किसी चीज को किसी तरीके से हमारी समझ से मिटा भी दिया तो भी हम पायेंगे कि वास्तव में कामना मिटी नहीं है। यह बात बहुत ही जटिल और गहन है। इसे वास्तव में समझ पाना सरल नहीं है। 'मैं निखैयगुण हो जाऊँ, या अहं से मुक्त हो जाऊँ', ये बातें केवल सुनने में ही अच्छी लगती हैं, जबकि व्यावहारिक तौर पर इनका वैसा स्वरूप होता नहीं है।
यदि श्रीमाँ को हमारे अहं की उपयोगिता है तो हमें उसे मिटाने पर आग्रह क्यों होना चाहिये? श्रीमाँ के एजेंडा (खण्ड २) में २ अगस्त १९६१ की वार्ता में हम पाते हैं कि जब एक बार भगवान् शिव श्रीमाँ के कक्ष में आए और मानव देह से स्वयं को बद्ध करने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने के बाद श्रीमाँ को कहा, "किन्तु आप जो कुछ भी चाहेंगी वह मैं आप को दे दूँगा।" श्रीमाँ ने कहाँ (हालाँकि यह वार्ता किसी प्रकार के उच्चारित शब्द के बिना थी) "मैं भौतिक अहं से मुक्त होना चाहती हूँ।" इससे आगे श्रीमाँ कहती हैं, "...ऐसा हो गया! यह अद्भुत था!... कुछ समय बाद मैं श्रीअरविन्द को खोजती हुई उनके पास गई और उनसे कहा, 'देखिये क्या हो गया है! मुझे कोशिकाओं के एक-दूसरे से अब और अधिक जुड़े न रहने का एक मजेदार संवेदन हो रहा है (श्रीमाँ हँसती हैं।) वे बिखरने वाली हैं!' उन्होंने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, अभी नहीं। और वह प्रभाव समाप्त हो गया।" चूँकि श्रीअरविन्द आश्रम, पांडिचेरी के संचालन के लिए भौतिक अहं आवश्यक था इसलिए श्रीअरविन्द ने इस प्रकार उसे समाप्त कर दिया। इसी प्रकार हमें इस विषय में समझ नहीं होती कि हमारी कामना, अहं आदि का श्रीमाँ के लिए क्या उपयोग है। इसलिए हमें न तो कामना से परहेज है और न ही अहं से। हम तो चाहते हैं कि हमसे इस तरह का काम न हो जिसमें श्रीमाँ की प्रसन्नता न हो। और यदि वे प्रसन्न हों तो फिर इन कामना आदि से कोई समस्या रहती नहीं। क्योंकि जितना ही अधिक हम इन्हें संयमित करने का प्रयास करते हैं उतने ही अधिक हम अपने-आप पर केंद्रित होते जाते हैं। इन सब बातों का समाधान एक ही है कि यदि भरसक प्रयत्न करने के बाद भी स्थिति अपने वश में न हो तो श्रीमाँ के हाथों में सौंप दो और वे स्वयं ही जो आवश्यक है वैसा करा लेंगी। इसलिए पढ़ी-पढ़ाई बातों में पड़कर कि, 'कामना नहीं होनी चाहिये, लोभ नहीं होना चाहिये, अहं को खत्म करना चाहिये', इनसे हमारा कोई लाभ नहीं है। करने योग्य काम तो एक ही है कि श्रीमाँ को समर्पण कर दिया जाए और जब, जहाँ और जैसा उन्हें उचित लगे वैसा वे स्वयं ही करा लें।
धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ।। ३८।।
३८. जिस प्रकार धूम से अग्नि, धूलि से दर्पण ढका होता है और जैसे झिल्ली से गर्भ ढका होता है उसी प्रकार काम से यह (ज्ञान) ढका होता है।
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ।। ३९।।
३९. और हे कौन्तेय! ज्ञानी के नित्य शत्रु और कभी भी तृप्त न होनेवाले अग्निरूप इस काम से ज्ञान ढका हुआ है।
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ।। ४०।।
४०. इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इसके आश्रय-स्थान कहे जाते हैं; इन्हें आश्रय बनाकर (इनमें स्थित होकर) ज्ञान को आच्छादित कर के यह देहधारी जीव को भ्रांत कर देता है, मूढ़ बना देता है।
सूक्ष्म अतीन्द्रिय प्राण संवेदनात्मक मन को आक्रांत कर के उसमें संवेदनों की अशान्ति ले आते हैं, क्रियाशील मन को यह प्राण प्रभुत्व, अधिकार, आधिपत्य एवं सफलता की लिप्सा से तथा प्रत्येक आवेग की परिपूर्ति की कामना से आक्रांत करता है, भावनात्मक मन को यह प्राण रुचि और अरुचि तथा राग और द्वेष के भावों को तृप्त करने की कामना से भर देता है, भयजनित जुगुप्साओं और आतंकों तथा आशाजनित आयासों और निराशाओं को जन्म देता है, शोक की यन्त्रणाओं तथा हर्ष के क्षणस्थायी ज्वरों एवं उसकी उत्तेजनाओं को हम पर लाद देता है, बुद्धि और उसके संकल्प को इन सब चीजों में सहापराधी बनाकर उन्हीं के ढंग से विकृत एवं पंगु यन्त्रों में परिणत कर देता है, अर्थात् संकल्प को लालसा की इच्छा में तथा बुद्धि को सीमित, अधीर और कलहरत पूर्वनिर्णय एवं मत आदि निम्न रूपों के पक्षपातपूर्ण, लड़खड़ाते हुए और एक आतुर अनुयायी में बदल डालता है।
यह बात स्पष्ट है कि कामना केवल कोई सतही चीज नहीं है : खाने-पीने या मौज-मस्ती आदि की इच्छा ही कामना नहीं है। कामना तो बहुत ही गहरी चीज है। यह संवेदनात्मक मन को आक्रांत कर के उसमें संवेदनों की अशान्ति ले आती है। संवेदन अर्थात् सुनना, देखना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, सूँघना। इनकी अशांति का अर्थ है कि दृष्टि संबंधी विकृतियाँ, स्वाद संबंधी आवेग, स्पर्श से संबंधित सभी प्रकार की भोग आदि की कामनाएँ। ये सारी विकृतियाँ हमें सारे दिन विचलित करती रहती हैं। इस प्रकार कामना संवेदनों के द्वारा भी आती हैं। ये सारी इन्द्रियाँ न केवल सतही चीजों में बल्कि गहरी चीजों में भी सहभागी होती हैं। जैसे सुनने की इंद्रिय - यह केवल कोई मधुर संगीत सुनने को ही नहीं बल्कि अपनी प्रशंसा सुनने को भी लालायित रहती है, जब कोई हमारी बुराई करता है तो बहुत बुरा लगता है। और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तो व्यक्ति कितने-कितने साधन कर लेता है। इसके लिए वह इतना लालायित रहता है कि इसके लिये वह ऐसी कोई बात करेगा, ऐसे शब्द बोलेगा, ऐसी चेष्टा करेगा जिससे कोई उसकी प्रशंसा करे। तो इसमें सुनने की इंद्रिय का प्रयोग केवल मधुर चीजें ही नहीं अपितु अपने-आप को सुहाती हुई चीजें सुनने के लिये भी होता है। इसी प्रकार सभी इंद्रियों के साथ है, क्योंकि सारी इन्द्रियों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, न ही जिस सूक्ष्म रूप से सभी चीजों में ये घुसी हुई हैं उसका ही कोई वर्णन किया जा सकता है। यह तो इतना बड़ा और इतने सूक्ष्म रूप से व्यवस्थित प्रपंच चल रहा है कि इसे पूरी तरह से समझा जा ही नहीं सकता। क्योंकि जब व्यक्ति विचलित हो रहा है, उस समय विवेकी रूप से सही-गलत का निर्णय करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उस समय व्यक्ति का विवेक, उसकी भेद करने की सामर्थ्य इन सभी चीजों से आच्छादित हो जाती है।
क्रियाशील मन को यह प्राण प्रभुत्व, अधिकार, आधिपत्य एवं सफलता की लिप्सा से तथा प्रत्येक आवेग की परिपूर्ति की कामना से आक्रांत करता है।
क्रियाशील मन जो कि सारे दिन यही सोचता है कि मैं क्या खरीद लूँ, क्या बेच दूँ, दुनिया में कोई अच्छा काम कर दूँ, किस तरीके से चीजों पर आधिपत्य कर लूँ आदि-आदि। इस प्रकार यह क्रियाशील मन सूक्ष्म रूप से क्रियाकलापों के अंदर प्रवेश कर जाता है और उन्हें प्रभावित करता है, उन्हें यंत्रवत् चलाता रहता है। जैसे व्यापारी यह सोचता है कि किस प्रकार से मेरा व्यापार और अधिक बढ़ सकता है, हम कोई अस्पताल चला रहे हों तो सोचते हैं कि किस प्रकार यह और भी बड़ा हो जाए, यदि कोई शिक्षा क्षेत्र में हो तो उसके अपने तरीके के मनसूबे होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने-अपने तरीके के मनसूबों से भरा रहता है। जब यह प्राण क्रियाशील मन को इतना आक्रांत कर लेता है तो इस प्रकार के क्रियाकलापों के बीच व्यक्ति को कहाँ कोई अच्छी चीज सोचने की फुर्सत रहेगी? पहले तो वह आवेगों से घिरा रहता है और उसके ऊपर फिर उसकी संतुष्टि के लिए इस क्रियाशील मन की क्रिया। यह सब कामनाओं का ज्वर है।
भावनात्मक मन को यह प्राण रुचि और अरुचि तथा राग और द्वेष के भावों को तृप्त करने की कामना से भर देता है,
रुचि और अरुचि, राग-द्वेष के साथ-ही-साथ प्राण के षड् रिपुओं में से एक रिपु मत्सर भी लगा रहता है। यह एक प्रकार की अहंकारमय प्रतिक्रिया है कि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज क्यों प्राप्त हो गई या फिर मुझसे बेहतर क्यों प्राप्त हो गई। उदाहरण के लिए यदि कोई दूसरा व्यक्ति मकान खरीद लेता है तो मन में भाव उठता है यह मकान उसने क्यों खरीद लिया यह तो मुझे खरीदना चाहिए था, यदि मैं गाड़ी से कहीं जा रहा हूँ तो दूसरा मेरे से आगे कैसे निकल गया जबकि मेरी तो गाड़ी भी बहुत अच्छी है। यदि मेरा दोस्त कक्षा में सबसे आगे रहता है तो यह भाव कि उसे सबसे अधिक अंक क्यों मिल गए, मुझे मिलने चाहिये थे। इस भाव से ग्रसित होकर तो लोग बहुत बार एक-दूसरे की हत्या तक कर डालते हैं। वास्तव में, मन और प्राण के अन्दर रुचि-अरुचि तथा अपना अहं बोध भरा रहता है। व्यक्ति का भावात्मक मन केवल इस दृष्टिकोण से देखता है कि सामने वाले व्यक्ति ने अच्छी बात कही या बुरी बात कही। उसे इसके अतिरिक्त अन्य किसी चीज के लिए अवकाश ही नहीं रहता। वही भावात्मक मन जो यदि गहराई में जाता तो व्यक्ति को भगवान् से जोड़ सकता था परन्तु वह इन बाहरी चीजों में इतना व्यस्त रहता है कि इन गहरी चीजों के लिए उसे तो क्षण भर का अवकाश ही नहीं रहता। सारे दिन व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने और सुख बटोरने में लगा रहता है। इसके अतिरिक्त तो उसे और कोई सरोकार रहता ही नहीं। व्यक्ति का प्राण एक विशेष प्रकार के लोगों से मिलने में, विशेष प्रकार की चीजों के स्पंदनों में रुचि लेता है और वह उसी प्रकार के लोगों से मिलना और बातचीत करना पसंद करता है, फिर वह चाहे उसके परिवार का हो, मित्र हो या रिश्तेदार हो। व्यक्ति अपने-आप से यह प्रश्न तक भी नहीं पूछता कि 'मुझे क्या करना चाहिए, और करना चाहिये भी या नहीं।'
भयजनित जुगुप्साओं और आतंकों तथा आशाजनित आयासों और निराशाओं को जन्म देता है,
और ये सब भय, निराशा, जुगुप्सा आदि अंदर चित्त से उठती हैं और व्यक्ति का जीवन उनसे भरा रहता है। यदि आपके मन में कोई इच्छा या कामना है कि अमुक चीज या कोई अभीष्ट चीज हो जाए, तो स्वतः ही इसके साथ ही भय तो निश्चित रहेगा ही कि यदि वह अभीष्ट या वांछित चीज न हुई तो? ये सारी चीजें व्यक्ति को चिन्ता, फिक्र से भर देती हैं। यदि उसके अन्दर कोई सफाई करने वाला तत्त्व न हो जो इन सब प्रभावों की शुद्धि करता हो, या इन सब चीजों को परिष्कृत करता हो तो व्यक्ति इन्हीं से ही भरा रहेगा।
बुद्धि और उसके संकल्प को इन सब चीजों में सहापराधी बनाकर उन्हीं के ढंग से विकृत एवं पंगु यन्त्रों में परिणत कर देता है,
बुद्धि इस जोड़-तोड़ से सोचती है कि कैसे मेरी योजना पूरी हो जाए, कैसे मैं अपने हेतु साध लूँ, किस प्रकार को मैं व्यवस्था करूँ कि मुझे रुचिकर चीज मिल जाए और इसके लिए कैसे मैं किसी को पटा लूँ, बहला-फुसला लूँ कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। और इस सबमें बुद्धि इन चीजों के लिए यन्त्र बन जाती है। बुद्धि तो केवल प्राण की कामनाओं की पूर्ति करने का यंत्र बन जाती है। उसका जो सही उपयोग है कि व्यक्ति को भले-बुरे का बोध, उचित-अनुचित मार्ग दिखा दे, वह तो रहता ही नहीं है। वह तो पंगु हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? सत्य की तो पूरी तरह से हत्या ही हो जाती है। इसीलिए सारा जीवन यों ही इन सब चीजों में चलता रहता है। सारा संसार इसी में लगा रहता है।
अर्थात् संकल्प को लालसा की इच्छा में तथा बुद्धि को सीमित, अधीर और कलहरत पूर्वनिर्णय एवं मत आदि निम्न रूपों के पक्षपातपूर्ण, लड़खड़ाते हुए और एक आतुर अनुयायी में बदल डालता है।
व्यक्ति की बुद्धि में एक विचार या एक पूर्वधारणा होती है कि अमुक चीज सही है और अमुक गलत है और उसी के ऊपर आग्रह कर के वह उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। वहीं, व्यक्ति की प्राण-शक्ति कहती है 'मैं सही हूँ और यह बात मैं दूसरे को समझा कर रहूँगा। और एक दिन वह भी यह देख लेगा और जान जाएगा और आकर कहेगा कि आप सही थे, मैं तो गलत कर रहा था।' इन सब बातों से प्राण को बड़ा सन्तोष मिलता है। अपार खुशी मिल जाती है उसे इस सारे व्यवहार में। 'मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं सही हूँ'। ये सारी चीजें हमें भरे रखती हैं और अपनी धुन पर नचाती रहती हैं। कौन है जिन्हें ये चीजें अछूता छोड़ देती हैं और सत्य से विचलित नहीं करतीं। हमारे साथ इन सब भागों की क्या क्रिया हो रही है, किस प्रकार ये सभी समय हमें आक्रांत कर के अपने हेतु सिद्ध करते हैं इसका यह बड़ा ही जीवंत वर्णन श्रीमाँ व श्रीअरविन्द की कृतियों में है।
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ।। ४१।।
४१. इसलिये हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन! तू पहले इन्द्रियों को नियंत्रित कर के ज्ञान और विवेक का नाश करनेवाले इस पापी (दुष्ट) काम को दृढ़तापूर्वक मार डाल।
कामना से छुटकारा पाने के लिए, जो कि अशुभ अथवा पाप और कष्ट का संपूर्ण मूल है... हमें कामना के कारण का अन्त करना होगा, विषयों को पकड़ने और उन्हें भोगने हेतु बाहर की ओर भागती इन्द्रियों को रोकना होगा। जब इस तरह से इन्द्रियाँ दौड़ पड़ने में प्रवृत्त हों तब विषयों से सर्वथा हटा कर उन्हें पीछे खींच लेना होगा...
धरती पर सभी शक्तियाँ अपने-आपको प्रकट करने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये शक्तियाँ अपने-आप को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से आती हैं और यदि तुम इनके बीच में कोई अवरोध खड़ा कर दो और प्रकट करने से इन्कार कर दो तो वे कुछ समय तक अवरोध के विरुद्ध टकराने का प्रयास कर सकती हैं, परंतु अंत में वे स्वयं को थका लेंगी और अभिव्यक्ति न मिलने के कारण वे लौट जाएँगी और तुम्हें चैन में छोड़ देंगी।
अतः तुम्हें ऐसा कभी न कहना चाहियेः "पहले मैं अपने विचार की शुद्धि करूँगा, अपने शरीर की शुद्धि करूँगा, अपने प्राण की शुद्धि करूँगा, और बाद में अपने कर्मों की शुद्धि करूँगा।" यही सामान्य क्रम है, पर यह कभी सफल नहीं होता। कारगर क्रम है बाहर से आरंभ करनाः "सबसे पहली चीज है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और उसके बाद, मैं अब और इसकी इच्छा भी न करूँगा, और उसके बाद मैं अपने सभी आवेगों के लिये अपने दरवाजे पूर्ण रूप से बंद कर दूँगाः मेरे लिये उनका अस्तित्व ही नहीं, अब मैं उनसे बाहर हूँ।" यही सच्चा क्रम है, ऐसा क्रम जो कारगर है। पहले, उसे करो मत। और तब तुम और अधिक इच्छा न करोगे और उसके बाद वह तुम्हारी चेतना से पूरी तरह से निकल जायेगी।
प्रश्न : गीता निग्रह और संयम की बात करती है। उससे यह अर्थ समझ आता है कि निग्रह करने में व्यक्ति उस क्रिया को अभिव्यक्ति तो प्रदान नहीं करता, पर उसके विषय में अंदर कामना या इच्छा बनी रहती है। जबकि संयम में व्यक्ति न तो उसे बाहर अभिव्यक्त ही होने देता है और न ही उसके विषय में सोचता ही है। तो क्या एक प्रकार से यह भी निग्रह ही नहीं हो गया? यदि इन्हें बौद्धिक रूप से देखा जाए तो इनके बीच का क्या संबंध है या क्या भेद है?
उत्तर : इस पूरे विषय को हमें एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अमुक काम नहीं करूँगा जबकि उसके निषेध के लिए उसके पास आवश्यक मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, तो उसे तो अवश रूप से उस कार्य को करने को बाध्य होना पड़ेगा। बिना इस मनोवैज्ञानिक आधार के वह इस निषेध को सिद्ध कर ही नहीं सकता। यदि व्यक्ति में निषेध करने की क्षमता है और साथ ही बुद्धि में भी वह उससे कुछ दूर हटने की क्षमता रखता है तो वह कुछ निषेध करने में सफल होगा, अन्यथा तो निषेध के द्वारा वह अपने-आप को उस चीज से या फिर इंद्रियों की तृप्ति से बलपूर्वक वंचित कर के अपने अंदर असंतुलन पैदा कर लेगा और जीवन में बड़ी भारी तकलीफ या संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी।
यहाँ यह नहीं कह रहे कि निग्रह गलत है। बल्कि यह कि संयम उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। अगर व्यक्ति संयम नहीं कर सकता, अपने मन को इंद्रिय विषय से लिप्त होने से दूर नहीं रख सकता, तब बात अलग है। यदि अंतरात्मा में इतनी ताकत है कि जब उससे 'संकल्प' आता है तो वह उस क्रिया और मन की उस इंद्रिय विषय से लिप्तता दोनों को ही संयमित तथा नियंत्रित कर सकता है तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। मन के निरर्थक विचारों का वह निषेध कर देगा और यदि वे आते भी रहें तो वह इतना समर्थ होगा कि उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे यह करने के लिए मन की सहायता या उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। उनके बिना भी वह संकल्प यह संयम साधित कर सकता है। साथ ही, इस संकल्प के द्वारा जो क्रिया होगी उससे सत्ता में ऐसा कोई असंतुलन नहीं आता जिससे कि व्यक्ति के जीवन में कोई संकट की स्थिति आए।
जब यह संकल्प या फिर यह गहरा हिस्सा प्रभावी नहीं हो, तब केवल निग्रह से तो व्यक्ति बड़ी तकलीफ में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास अपने सहारे या समर्थन के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए ऐसा निग्रह अधिक समय तक टिक पाना मुश्किल है।
दूसरे यदि व्यक्ति में संयम करने की क्षमता है तो वह यह काम अधिक आसानी से कर सकता है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें संभव है कि मन-बुद्धि का संयम न भी हो पर आंतरिक संकल्प इतना सुदृढ़ हो कि अंदर आत्मा से कोई बात आ जाती है और मन-बुद्धि के किसी प्रकार के सहारे के बिना ही यह काम साध देती है। साथ ही, यह संयम आरंभ में सभी चीजों पर लागू करना तो मुश्किल है। इसे हमें कुछ चुनिंदा चीजों के ऊपर लागू करना होगा। कामना तो व्यक्ति के रोम-रोम में घुसी हुई है। इसलिए उसे आरंभ में ही व्यक्ति पूरी तरह से कैसे निकाल सकता है। उसे तो इस तरह किसी भी तरीके से निकाला जा ही नहीं सकता। पर इस सब में सब कुछ व्यक्ति की सच्चाई पर निर्भर करता है। क्योंकि जब यदि यह नजर आ जाए कि कोई क्रिया गलत है तब फिर उस पर नियंत्रण या संयम कैसे किया जाए? तो उसके लिए तो व्यक्ति को कृतसंकल्प होकर अपनी सारी शक्ति लगानी होगी और उसे रोकना ही होगा। यदि व्यक्ति की अंतरात्मा इतनी शक्तिशाली है तो वह उसे मिटा सकेगा। और यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है तब फिर उसके संयम की दिशा में कोई निर्णायक पग नहीं लिया जा सकेगा और कशमकश चलती रहेगी।
वास्तव में श्रीमाताजी जो कह रही हैं वह शक्तिशाली संकल्पशक्ति के बारे में है। और साथ ही, यह संकल्प किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं पर लागू हो सकता है, क्योंकि कामना का हमारी सत्ता में प्रवेश तो बड़े सूक्ष्म रूप से भी है इसलिए यह प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है और इसे समझने में और इसका समाधान करने में बहुत समय लगता है। यदि किसी की अंतरात्मा पर्याप्त विकसित हो चुकी है तो यह कार्य अपेक्षाकृत कम समय में किया जा सकता है, अन्यथा हो सकता है कि इसमें बहुत लंबा समय लगे, संभव है पूरा जीवन ही लग जाए और तब भी पूरा न हो। यह व्यक्ति की अंतरात्मा की स्थिति पर निर्भर करता है। और इसके लिए व्यक्ति को साधना पथ पर चलना होगा।
व्यक्ति कर्मयोग, भक्तियोग, या ज्ञानयोग या फिर इनके किसी मिले-जुले रूप में से कौनसा पथ अपनाता है, या फिर केवल समर्पण भाव ही अपनाता है, यह व्यक्ति के गठन पर निर्भर करता है। परंतु यह संयम, यह शुद्धिकरण एक उत्तरोत्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बहुत से धोखे, जाल-घात हैं। प्रत्येक कामना के पीछे ही ऐसा प्रतीत होगा कि कोई अच्छी चीज है। साथ ही भगवान् का संकल्प भी अपने कार्य के लिए कामना के रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए इस भगवद्-इच्छा में और कामना में भेद कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारा मामला ही जटिल हो जाता है। इसमें कुछ चीजों पर तो व्यक्ति अपनी संकल्प-शक्ति लागू कर सकता है जैसे कि उसे बीड़ी-सिगरेट का सेवन नहीं करना है, या कोई नशा नहीं करना है। परंतु यदि कोई कहे कि एकाएक ही वह अपने अंदर की कामना को निकाल बाहर करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि व्यक्ति कामना के विषय में सचेतन ही नहीं होता कि किस प्रकार उसके रोम-रोम में वह घुसी हुई है। इसके विषय में सचेतन होने में भी जीवन लग जाता है कि किस प्रकार कामना रोम-रोम में घुसी हुई है।
दूसरी बात यह है, कि जब व्यक्ति परम की ओर बढ़ रहा होता है तब यह समझ पाना और भेद कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है कि उसमें कैसी-कैसी कामनाएँ, इच्छाएँ और उनके मिश्रण भरे हुए हैं। मन-बुद्धि से कामनाओं आदि के विषय में उसके द्वारा ऐसा कोई रुख अपनाए जाना और इस बारे में योजनाएँ बनाए जाना कि इन्हें हटाने का अमुक तरीका अच्छा है, अमुक उतना प्रभावी नहीं है, अपनी जगह ठीक है, पर अंततः गीता कहती है 'सर्वधर्मान्परित्यज्य'। अतः सार यही है कि साधना के संबंध में हमारे के जितने भी दृष्टिकोण, जितने भी मानदण्ड हैं उन सब को त्याग कर सीधे सभी कुछ श्रीमाताजी के हाथों में सौंप दें। केवल वे ही जानती हैं कि कौनसी चीज कहाँ, कैसे और कितनी बची रहनी चाहिये और कौनसी नहीं। हमने जिन्हें इच्छा, कामना, संकल्प, अभीप्सा आदि जो-जो मान रखा था उनके विषय में सही रूप में तो केवल वे ही जानती हैं कि वास्तव में कौनसा क्या है और किसे रखना है या त्याग देना है। उनके हाथों में सौंप देने पर उनकी क्रिया इन सभी क्रियाओं से परे चली जाती है। वास्तव में यह समर्पण का पथ ही राजमार्ग है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति यथासमय आवश्यक उचित कर्म नहीं करेगा। क्योंकि ये सभी चीजें उसका अंग ही हैं। यदि व्यक्ति को सच्चा शुद्धिकरण, सच्चा परिवर्तन साधित करना है, परमोच्च की ओर जाना है तो समर्पण का राजमार्ग अपनाना होगा क्योंकि किसी भी मापदण्ड के सहारे व्यक्ति कोई आंशिक चीजें भले ही प्राप्त कर ले, परंतु अंततः तो ऐसा सर्वांगीण समर्पण करना ही होगा जिसमें व्यक्ति के अंदर और कोई दूसरी प्रेरणा रहती ही नहीं। इसी राजमार्ग की ओर चलना होगा, इसके अतिरिक्त सच्ची संसिद्धि का और कोई मार्ग है ही नहीं। बाकी तो किसी-न-किसी निम्न सूत्र में ही बँध कर रह जाना है। गीता का मूलभाव भी इसी समर्पण का है।
आरंभ में व्यक्ति अपने किसी एक मानदण्ड को अपनाकर कोई सामान्य कार्यक्रम के अनुसार आगे चल सकता है जिसमें वह तय कर सकता है कि अमुक काम उसे करने हैं और अमुक त्याग देने हैं। हर व्यक्ति का यह कार्यक्रम उसके गठन के अनुसार भिन्न-भिन्न होगा। परंतु यदि व्यक्ति का संतुलन इस प्रकार का है, उसके अंदर की पुकार ऐसी है कि उसे पूरी यात्रा तय करनी है, तो वह समर्पण के इस राजमार्ग पर आ ही जाएगा और इसे अपना ही लेगा जिसमें कि अपने सभी मापदण्ड, दृष्टिकोण, तौर-तरीके, अपनी सभी धारणाएँ, पूर्वाग्रह आदि सभी श्रीमाताजी के हाथों में सौंप दिये जाते हैं और उन्हें इनका जो उपयोग करना है और व्यक्ति से जो कराना है वह वे स्वयं ही करा लेंगी। व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना होगा कि इस मार्ग में वह धोखा खा सकता है और निश्चित खाएगा ही। प्रायः व्यक्ति इसका स्पष्टिकरण देता है कि श्रीमाँ कि ऐसी इच्छा थी इसलिए ऐसा हो गया। हालाँकि वह धोखा खाना भी साधना का ही अंग है। परंतु इन सब के होते हुए भी यदि व्यक्ति में यह श्रद्धा आ गयी कि वास्तव में जो कुछ भी होता है, श्रीमाँ जैसा करती हैं या कराती हैं उनका अपना विधान है और हर एक बात में, हर एक चीज में श्रीमाँ का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य निहित होता है, तब फिर व्यक्ति मार्ग पर अग्रसर होता जाता है।
अब गीता में भगवान् अर्जुन को कहते हैं कि इस काम रूपी शत्रु को मार, परंतु प्रश्न तो यह है कि वह उसे मारेगा कैसे? उस प्रश्न का गीता अब उत्तर देगी।
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ।। ४२।।
४२. वे कहते हैं कि इन्द्रियाँ (उनके विषयों से) ऊपर (परं) होती हैं, इन्द्रियों से मन ऊँचा होता है और मन से बुद्धि ऊँची होती है; और जो बुद्धि से परे है वह है पुरुष।
हमें सांख्यों की उस मनोवैज्ञानिक क्रमव्यवस्था को याद रखना चाहिये जिसे गीता स्वीकार करती है। इस क्रमव्यवस्था में एक ओर पुरुष है जो स्थिर, अकर्ता, अक्षर, एक और अविकसनशील या अपरिवर्तनशील है; दूसरी ओर प्रकृति है जो सचेतन पुरुष के बिना स्वयं जड़ निष्क्रिय है, जो कीं तो है परंतु इसका यह कर्तृत्व पुरुष की चेतना के सान्निध्य से, उसके संपर्क में आने से ही है, जैसा कि हम कहेंगे, पहले एक नहीं अपितु अपरिमित, त्रिगुणात्मिका, विस्तरण (evolution) एवं अंतर्वलयन (involution) में सक्षम है। पुरुष और प्रकृति का संपर्क ही आत्मनिष्ठता (subjectivity) और वस्तुनिष्ठता (objectivity) के खेल को उत्पन्न करता है, जो कि हमारी सत्ता का अनुभव है; जो हमारे लिए आत्मनिष्ठ अथवा अंतरंग है पहले वह विकसित होता है, क्योंकि पुरुष-चेतना अथवा आत्म-चेतना ही प्रथम कारण है, और जड़ प्रकृति-शक्ति केवल द्वितीय और पहले पर आश्रित कारण है; तथापि यह प्रकृति ही है, न कि पुरुष, जो हमारी आत्मनिष्ठता या व्यक्तिपरकता के उपकरणों की आपूर्ति करती है। इस क्रम में सर्वप्रथम है बुद्धि अर्थात् प्रकृति-शक्ति से विकसित होती विवेकशील और निर्णयकारी शक्ति, और बुद्धि के साथ विकसित होती अपने को दूसरों से पृथक् करने वाले अहंकार की शक्ति। तब इस विकास के द्वितीय क्रम में इन बुद्धि और अहंकार में से इंद्रिय-मन या मनस् की शक्ति उत्पन्न होती है जो विषयों की पृथक् पृथक् पहचान करता है। यहाँ हमें भारतीय नामों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द सचमुच उनके पर्याय नहीं हैं; इस विकास के तीसरे क्रम में इंद्रिय-मन में से दस विशिष्ट इंद्रियाँ प्राप्त होती हैं, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ, तदनंतर ज्ञानेन्द्रियों की शक्तियाँ अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न होते हैं, जो हमारे मन के लिये स्थूल विषयों का मूल्य निर्धारित करते हैं और हमारी आत्मनिष्ठता में पदार्थों की जो प्रतीति होती है वह उन्हीं के द्वारा होती है। इन्हीं पाँच विषयों के उपादान-स्वरूप पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, जिनके विभिन्न सम्मिश्रणों से बाह्य जगत् के पदार्थ उत्पन्न होते हैं।
प्रकृति के गुणों की ये अवस्थाएँ और शक्तियाँ पुरुष की विशुद्ध चेतना में प्रतिभासित होकर हमारे अशुद्ध अंतःकरण के उपादान बनती हैं, अशुद्ध इसलिए कि इसका कार्य बाह्य जगत् के अनुभवों और अंतःकरण पर होनेवाली उनकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है। यही बुद्धि- जो मात्र निर्णायक शक्ति है और जो अपनी अनिश्चित निश्चचेतन शक्ति में से सब जड़वत् निर्णय किया करती है - हमारे लिए मेधा और संकल्प का रूप ले लेती है। मनस्, जो एक निश्चेतन शक्ति है, प्रकृति के भेदों को बहिरंग क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा ग्रहण करता और आकर्षण के द्वारा उनसे संलग्न होता है, इन्द्रियानुभव और कामना बनता है जो बुद्धि और संकल्प के ही दो भौंडे या विकृत रूप हैं, - यही इंद्रिय-मन संवेदनात्मक, भावावेगात्मक और स्वैच्छिक या इच्छाप्रधान बनता है, इच्छाप्रधान से यहाँ अभिप्रेत है निम्नकोटि की इच्छा, आशा, उत्कंठा, कामनामय आवेश, प्राणिक आवेग, और ये सबके सब संकल्प-शक्ति के ही विकार हैं। इन्द्रियाँ इस इंद्रिय-मन का उपकरण बनती हैं, जिनमें इंद्रियगम्य-ज्ञान की पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, और हमारे आवेगों और प्राणिक अभ्यासों की पाँच सक्रिय कर्मेन्द्रियाँ जो अंतरंग जगत् और बहिरंग जगत् के बीच मध्यस्थ का काम करती हैं; बाकी सब हमारी चेतना के विषय, इन्द्रियों के विषय हैं।
स्थूल जगत् के विकास का जैसा क्रम हम देखते हैं उससे यह क्रम विपरीत प्रतीत होता है। परन्तु यदि हमें स्मरण हो कि स्वयं बुद्धि भी अपने-आप में जड़ प्रकृति की एक जड़ क्रिया है और इस अर्थ में निश्चय ही परमाणु में भी एक अचेतन संकल्प और प्रज्ञा, भेदकारी और निश्चयकारी शक्ति होती है, यदि हम यह देखें कि पौधों में भी, जीवन के इन अवचेतन रूपों में भी, संवेदन, भावावेग, स्मृति और आवेगों के असंस्कृत अचेतन उपादान मौजूद हैं और फिर यह देखें कि प्रकृति की ये शक्तियाँ ही किस प्रकार आगे चलकर पशु और मनुष्य की विकासोन्मुख चेतना में अंतःकरण के रूप धारण करती हैं, तो हमें यह पता लगेगा कि आधुनिक विज्ञान ने जड़ प्रकृति के निरीक्षण द्वारा जो कुछ तथ्य प्राप्त किया है, उसके साथ सांख्य प्रणाली का मेल मिल जाता है। जीव के प्रकृति से लौटकर पुनः अपने पुरुष-स्वरूप को प्राप्त करने के विकास-क्रम में प्रकृति-विकास के मूल क्रम का उल्टा क्रम अपनाना पड़ता है। उपनिषदों ने तथा उपनिषदों का ही अनुसरण कर के और लगभग उपनिषदों के वचनों को ही उद्धृत कर के गीता ने हमारे अंतःकरण की शक्तियों का आरोहणक्रम इस प्रकार बतलाया है- 'अपने विषयों से इन्द्रियाँ परे हैं, इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे जो है वह, 'वह' है' - चिदात्मा, परम् पुरुष। इसलिए गीता कहती है, इस पुरुष को, हमारे आत्मनिष्ठ जीवन के इस परम् कारण को हमें बुद्धि के द्वारा समझना और जान लेना होगा; उसी में अपने संकल्प को स्थिर करना होगा। इस प्रकार हम प्रकृतिस्थ निम्नतर अंतरंग पुरुष को उस महत्तर चेतन पुरुष की सहायता से सर्वथा संतुलित और स्थिर कर के अपनी शांति और आत्म-प्रभुत्व के अशांत और सदा-चंचल रहने वाले शत्रु, मन की 'कामना', को नष्ट कर सकेंगे।
भगवान् ने काम रूपी शत्रु को मार डालने का उपाय बता दिया है। परंतु केवल विचारों से संयमित नहीं करना है, क्योंकि स्वयं विचारों को भी नियंत्रित और संयमित करना होता है। उन्हें रोकने के लिए पीछे संकल्प की आवश्यकता है। इसे संसिद्ध करने के लिए किसी अधूरे तरीके से नहीं बल्कि पूरी तरह से ही इसे करना होगा। इसके लिए जो संकल्प है वह यदि अक्षर पुरुष में प्रतिष्ठित हो, तभी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है अन्यथा नहीं। अर्जुन को भगवान् ने यही उपाय बताया है। पहले अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से मन को सभी इंद्रियों के विषयों से हटाकर अक्षर पुरुष में स्थित किया जाए। गीता इस विषय को अभी और भी आगे विकसित करेगी। इस प्रकार अर्जुन को भगवान् ने यह एक मार्ग बताया है। वास्तव में अर्जुन को धीरे-धीरे यह समझाने का प्रयास है कि इन सब चीजों का कितना विकट स्वरूप है। और किस प्रकार इन कामनाओं-इच्छाओं आदि को जो कि हमारी शत्रु हैं - रोकने के लिए व्यक्ति को गहराई में निहित जो सत्य है वहाँ जाना होगा।
यहाँ भगवान् अर्जुन से कह रहे हैं कि गहराई में एक ऐसी चीज है जिसमें यदि तुम संकल्प करोगे तभी इन काम आदि शत्रुओं को रोक सकते हो, अन्यथा नहीं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि ऐसी शिक्षा देने मात्र से ही अर्जुन इन्हें रोक पाने में समर्थ हो जाएगा। और यहाँ यह उद्देश्य भी नहीं है। यहाँ तो उसे वे एक बुद्धि को उद्भासित करने वाली प्रकाशक और ऊपर उठाने वाली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिससे कि उसे मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात के लिए तैयार करें कि वह अधिक गंभीर चीजों के प्रति खुल सके ताकि उसे वह परम वचन 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' प्रभावी रूप से प्रदान किया जा सके। उसी परम वचन के लिए यह सारी तैयारी है। उससे पहले की जितनी भी शिक्षा दी जा रही है वह तो गीता के उस परम रहस्य को दिये जाने की योजना का ही अंग है।
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ।। 43 ।।
४३. हे महाबाहो अर्जुन ! इस प्रकार बुद्धि से भी परे जो उच्चतम तत्त्व (पुरुष) है उसे (बुद्धि के द्वारा) जानकर, महत्तर आत्मा के द्वारा निम्नकोटि के स्व को स्थिर निश्चल कर के कठिनाई से पकड़ में आने वाले कामनारूप शत्रु को मार डाल।
एक 'शक्ति' जो ऊँचाइयों पर रहती है, उसे क्रिया करनी होगी, जीवन के बंद कक्ष में अविनाशी की श्वास लानी होगी और सांत को 'अनंत' से परिपूरित करना होगा। जो कुछ भी अस्वीकार करे उसे, विदीर्ण कर नष्ट-भ्रष्ट कर देना होगा, और उन अनेक लालसाओं को कुचल डालना होगा जिनके हेतु हम उस एकमेव को गँवा देते हैं जिसके लिए हमारा जीवन बना था।
ऐसा माना जाता है कि कामना मानव-जीवन की वास्तविक प्रेरकशक्ति है और इसे निकाल फेंकने का अर्थ होगा जीवन के स्रोतों को बन्द कर देना; कामना की तृप्ति ही मनुष्य का एकमात्र भोग है और इसका उन्मूलन करने का अर्थ निवृत्तिमार्गीय वैराग्य के द्वारा जीवन की उमंग को ही शान्त कर देना होगा। परंतु आत्मा के जीवन की वास्तविक चालक-शक्ति है संकल्पशक्तिः कामना तो केवल हावी हुए शारीरिक जीवन और स्थूल मन में संकल्पशक्ति की एक विकृति मात्र है। जगत् पर स्वत्व प्राप्त करने तथा उसका उपभोग 'करने की आत्मा की मूल प्रवृत्ति आनन्द प्राप्त करने की उसकी इच्छाशक्ति में निहित है, और कामना की तृप्ति का भोग तो आनन्द-प्राप्ति की इच्छा का प्राणिक एवं शारीरिक विकृत-रूप है। यह अति आवश्यक है कि हम शुद्ध इच्छाशक्ति या संकल्प तथा कामना अर्थात् आनन्द-प्राप्ति की आन्तरिक इच्छा और मन तथा शरीर की बाह्य वासना एवं कामना में भेद को जानें। यदि हम अपनी सत्ता के अनुभव में व्यावहारिक रूप से यह भेद करने में असमर्थ रहते हैं तो हम या तो केवल एक जीवन-घाती वैराग्य में या जीने की स्थूल इच्छा में से किसी एक का चयन ही कर सकते हैं या फिर इन दोनों में एक भद्दा, अनिश्चित और अस्थिर समझौता करने का यत्न कर सकते हैं। वस्तुतः अधिकतर लोग यही करते हैं; बहुत थोड़े लोग जीवन की सहज-प्रवृत्ति को कुचलकर तपश्चर्यात्मक पूर्णता के लिये यत्न करते हैं; अधिकांश लोग जीने की स्थूल इच्छा का अनुसरण करते हैं, ऐसा वे कुछ ऐसे परिवर्तनों और प्रतिबन्धों के साथ करते हैं जिन्हें समाज उन पर लागू करता है या जिन्हें अपने-आप के मन तथा कार्यों पर लागू करने के लिए साधारण सामाजिक मनुष्य को शिक्षा दी गयी है; अन्य लोग नैतिक आत्मसंयम तथा कामनामय मानसिक एवं प्राणिक सत्ता की संयमित तृप्ति के बीच एक प्रकार के संतुलन का आदर्श स्थापित करते हैं और इस सन्तुलन में अविक्षिप्त मन तथा स्वस्थ मानव-जीवन के सुनहरे मध्यम मार्ग का दर्शन करते हैं। परन्तु इनमें से कोई भी तरीका जिस पूर्णता - अर्थात् जीवन में संकल्पशक्ति का भागवत् साम्राज्य - की हम खोज कर रहे हैं, वह नहीं प्रदान करता। प्राण अर्थात् प्राणमय सत्ता को सर्वथा कुचल डालने का अर्थ है जीवन की उस शक्ति का ही उच्छेद कर डालना जिसके द्वारा मनुष्य में स्थित देहधारी आत्मा का अधिकतर कार्य-कलाप पोषित होता है; जीने की स्थूल इच्छा को तृप्त करने का अर्थ है अपूर्णता से तुष्ट बने रहना; इनमें समझौता करने का अर्थ है आधे रास्ते में ही रुक जाना और न तो भूतल पर अधिकार पाना न स्वर्ग पर। परंतु यदि हम कामना के द्वारा अविकृत शुद्ध संकल्पशक्ति को अधिकृत कर सकें - और हम पाएँगे कि वह कामना की भड़क उठने वाली, धुँए से दबी-घुटी, शीघ्र क्लान्त एवं पराजित हो जानेवाली ज्वाला से कहीं अधिक स्वतन्त्र, शान्त, स्थिर और प्रभावपूर्ण शक्ति है, - और वासना के किसी भी विक्षोभ से पीड़ित या सीमित न होनेवाले आनन्द की शान्त आन्तरिक इच्छा को अधिकृत कर सकें तो हम प्राण को मन पर अत्याचार तथा आक्रमण करनेवाले शत्रु से परिवर्तित कर के एक आज्ञाकारी यन्त्र में बदल सकते हैं। इन महत्तर शक्तियों को, भी हम चाहें तो कामना के नाम से पुकार सकते हैं, पर तब हमें यह मानना होगा कि एक दिव्य कामना भी है जो प्राण की लालसा से भिन्न वस्तु है, एक ईश्वर-कामना भी है जिसकी यह अन्य एवं निम्नतर कामना एक अन्धकारमय छाया है और जिसमें इसे रूपान्तरित करना होगा। परंतु जो वस्तुएँ अपने स्वरूप तथा आन्तरिक क्रिया में सर्वथा भिन्न हैं उनके लिये भिन्न नाम रखना ही अधिक अच्छा है।
अब इस समस्या को हल किया गया है कि आखिर कामनाएँ आती कहाँ से हैं। वास्तव में, हमारे अंदर आत्मा कुछ अभिव्यक्त करना चाह रही है, उसी से ये सारी चीजें उद्भूत होती हैं, सतह पर तो ये चीजें उत्पन्न नहीं हो सकतीं क्योंकि सभी चीजों के लिए ऊर्जा और शक्ति तो आत्मा से ही प्राप्त होती है। अतः, सभी चीजों का मूल स्रोत तो वही है। पर जैसे हवा अपने मार्ग में अच्छी या बुरी गंध साथ ले लेती है, वैसे ही जब ये सभी भाव, उत्प्रेरणाएँ आदि तथा अन्य बहुत सी चीजें व्यक्ति के मन, प्राण तथा शरीर के माध्यम से आती हैं, और जैसा इन मन-प्राण-शरीरादि का गठन है, वैसी छाप उन चीजों के ऊपर लग जाती है। इसलिए वे ही चीजें जो मूल रूप से जिस स्वरूप और उद्देश्य को लेकर आत्मा से चलीं थीं, वे इन सब छापों के कारण अपना स्वरूप और उद्देश्य खो बैठती हैं। जितनी इन बाहरी हिस्सों में कम विकृति होती है उतनी कम विकृत छाप लगती है। परंतु चूंकि इन सभी भागों को भी रूपांतरित करना है इसलिए इन सभी संभावनाओं को बाहर आने का मौका प्रदान करना ही होगा। वैसे ही जैसे किसी बच्चे को कुछ सिखाने के लिए उसे त्रुटियाँ करने की कुछ छूट देनी ही होगी, उसी प्रकार इन यंत्रों को इस क्रमविकास में दिव्य विधान के द्वारा छूट दी गई है। अतः कामना मन, प्राण तथा शरीर में अपनी छाप लगा देती है। शरीर में भोगेच्छा, प्राण में कामनाएँ-वासनाएँ, तथा इन्हीं के कुछ अन्य अधिक सूक्ष्म रूप भी हैं, मन के अंदर अपने विचार हैं। ये सभी चीजें आत्मा से आते भावों, उत्प्रेरणाओं, संकेतों आदि के साथ जुड़ जाती हैं और आत्मा से आती चीजों का जो प्रयोजन था वह आच्छादित हो जाता है, विकृत हो जाता है, और इस सब का व्यक्ति को आभास तक भी नहीं हो पाता। तो इसका समाधान क्या है? यह सारा खेल इतना असुधार्य है, कामना आदि इतनी सूक्ष्म होती हैं कि बहुत अधिक प्रयत्न करने पर भी ये व्यक्ति को धोखा दे देती हैं। क्योंकि इन सबके साथ अहम् मिला होता है जो व्यक्ति की सभी चीजों को सही सिद्ध करने का काम करता है। कितने लोग हैं जिनका मानना है कि वे तो गीता का कर्मयोग ही कर रहे हैं। दूसरे लोगों को दूसरा भ्रम होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि लगभग सभी पूरी तरह से धोखे में होते हैं।
अतः कुछ ने यह दृष्टिकोण अपना लिया कि यह सब प्रपंच ही बेकार है, और इसको सुधारना लगभग असंभव है इसलिए अच्छा यह है कि व्यक्ति सब कर्मों का ही त्याग कर दे, ध्यान आदि तरीकों से केवल आत्मा में ही निवास करे, भगवान् का साक्षात्कार करे और अपने आत्मतत्त्व में ही रहे क्योंकि वहीं सब सुख मिल सकते हैं। और केवल वे ही कर्म करे जो शरीरचर्या के लिए अपरिहार्य हैं, और जब शरीर छूट जाए तो व्यक्ति इस प्रपंच में से छूट निकले। पारंपरिक आध्यात्मिकता में प्रतिपादित यह एक प्रचलित समाधान है, जो कि आत्मा के अपने-आप को इस पार्थिव जगत् में अभिव्यक्त करने के प्रयोजन को उचित नहीं ठहराता। हालाँकि जिसकी आत्मा की यही पुकार हो उसके लिए तो यह समाधान अनुकरणीय हो सकता है परंतु अधिकतर के लिए यह समाधान लागू नहीं होता क्योंकि उनकी आत्मा तो यहाँ किसी संसिद्धि के उद्देश्य से आई होती है।
कुछ दूसरों ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि यह प्रपंच जैसा है वैसा है। इसके विषय में विश्लेषण कर के व्यक्ति निरर्थक ही परेशान भले ही हो सकता है जबकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इसलिए ऐसे में तो भगवान् से प्रार्थना करने का रुख अपनाना चाहिये और जैसे भी यह सब प्रपंच चलता है वैसे चलता रहे, इससे कोई सरोकार न रखा जाए। जैसे-जैसे हमें अनुभव अर्जित होते जाएँगे हम इसे कुछ थोड़ा-बहुत समझ जाएँगे तो फिर समस्याएँ सूक्ष्म होती जाएँगी। और इसी प्रकार यह प्रपंच चलता रहेगा। इसलिए अच्छा हो कि व्यक्ति बिना बात ही परेशान न हो और सुख से जीए। यह एक दूसरा समाधान है।
तीसरा दृष्टिकोण यह है कि कुछ चीजों का तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि ये गलत हैं, ऐसी गलतियों को तो व्यक्ति अपनी इच्छाशक्ति के दबाव से रोके। बाकी चीजों का पता लगता नहीं है इसलिये उन्हें चलने दिया जा सकता है। यह मध्य मार्ग है जिसमें व्यक्ति कोई पापपूर्ण व्यवहार नहीं करता, समाज के नैतिक आदशों का सम्मान करता है और उनके अनुसार चलता है जिससे कि उसे सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की और अपनी निजी श्रेष्ठता के बोध की तृप्ति प्राप्त हो जाती है। इनके अतिरिक्त इंद्रियों की क्रिया तो जैसा उनका प्रकृतिगत गठन है उसके अनुसार चलती ही रहेगी, वह रुकेगी नहीं। इसलिए अच्छा है कि व्यक्ति उसमें अपनी ऊर्जा न गँवाए और उसे अपने तरीके से चलने दिया जाए। यह एक अलग समाधान है।
परंतु श्रीअरविन्द का कहना है कि हम यहाँ धरती पर भगवान् का शासन लाना चाहते हैं इसलिए हमारे लिए इनमें से कोई भी समाधान उचित नहीं है। हम यहाँ अपनी आत्मा की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। और इसका एक ही रास्ता है - इसे करने का दृढ़-संकल्प और जहाँ व्यक्ति को व्यक्तिगत पुरुषार्थ का स्थान दिखाई देता है वहाँ पूरे मनोयोग के साथ उसका प्रयोग करे और देखे कि वह कहाँ तक ले जाता है। और वह भी करने के साथ-साथ व्यक्ति को श्रीमाँ के प्रति खुलना चाहिये। धीरे-धीरे व्यक्ति को बोध होने लगता है। धीरे-धीरे जो भागवत् संकल्प अभिव्यक्त होना चाह रहा है उसमें मन-प्राण-शरीर की विकृति कम होती जाएगी, इच्छाएँ-कामनाएँ तो आरंभ में रहेंगी पर जैसे-जैसे उस संकल्प का प्रभाव सत्ता में बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे मन-प्राण-शरीर की विकृति कम होती जाएगी। तब फिर व्यक्ति अपनी कामना के विपरीत भी काम कर पाएगा। पसंद-नापसंद से हट कर, लाभ-हानि के विचार को अनदेखा कर भी काम कर सकेगा। यह सब क्रिया क्रमशः होने लगेगी। और जब समय आएगा तब व्यक्ति श्रीमाँ के, भगवान् के संकल्प से जुड़ जाएगा। और जब प्रभु के संकल्प से व्यक्ति जुड़ जाएगा तभी वह दिव्य कर्म कर सकेगा। यदि कर्मों का त्याग ही समाधान होता और यदि दिव्य कर्म संभव ही नहीं होते तब तो भगवान् कृष्ण अर्जुन को इस घोर कर्म में नियोजित ही क्यों करते? अर्जुन तो आरंभ में ही उससे पलायन की वृत्ति रख रहा था। यदि वन में जाकर तपस्या करना, कमाँ को छोड़ देना, जीवन से पलायन करना ही गीता की शिक्षा होती तो शेष सभी अध्यायों का तो कोई अर्थ ही नहीं था जिनके बाद कि भगवान् उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं।
सारी गीता का विकासक्रम इसी प्रयोजन से है कि अर्जुन इन सभी चीजों से ऊपर उठ जाए, भागवत् कर्म कर सके। यही सच्चा समाधान है, कि सत्ता पर भागवत् शासन को लागू किया जाए। ताकि बिना विचलित हुए, भगवद्-उद्देश्य से ही हम सभी कर्मों को कर सकें। कामना हमें विचलित करती है। यदि हमारी कोई अपनी पसन्द या नापसन्द है तो हम उसी के अनुसार कर्म करेंगे और इस कारण श्रीमाँ हमसे जो कराना चाहेंगी वह तो हम कर ही नहीं पाएँगे।
कामना आदि भगवान् के प्रति द्वेष भाव रखते हैं और कोई भी भागवत् कार्य नहीं होने देना चाहते। इसलिये यदि हम उन्हें प्रश्रय प्रदान करते हैं तो भागवत् कार्य की आशा कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमने तो अपने शत्रु को अपने ही घर में आश्रय प्रदान किया होता है। हमें यह संकल्प करना होगा कि वही कार्य करेंगे जो श्रीमाँ हमसे कराना चाहेंगी, भले ही वह कार्य हमें अच्छा लगे या न लगे। उस कार्य में यदि किसी को कामना नजर आती है तो उससे भी हमें कोई सरोकार नहीं है। इस प्रकार धीरे-धीरे मार्ग पर व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे व्यक्ति कोई एक योजना बना कर, या कोई एक मानसिक सूत्र पकड़ कर संसिद्ध कर पाए। जब व्यक्ति भागवत् शासन की स्थापना का तथा अपने-आप को श्रीमाताजी को समर्पित करने का संकल्प करता है तब उस शासन की स्थापना के लिए जो आवश्यक है उसे वह नहीं समझ सकता। परंतु श्रीमाताजी स्वयं ही अपने तरीकों से उसे उस ओर ले जाएँगी। इस सब प्रक्रिया में बीच में कामनाएँ भी 3pi उनका वर्जन भी आएगा, लिप्तता भी आएगी, उससे दूर हटने की क्रिया भी आएगी, निषेध, नकारात्मकता आदि न जाने क्या-क्या आएँगे। इन सब से होते हुए श्रीमाँ हमारे गंतव्य की ओर हमें ले चलेंगी। और जब धीरे-धीरे व्यक्ति इन सब चीजों से कुछ मुक्त होगा तब दिव्य कर्म संपादित होंगे, उससे पहले नहीं। भगवान् कहते हैं कि 'जन्म कर्म च मे दिव्यं' अर्थात्, भगवान् अवतार लेते हैं तो उनके जन्म और कर्म सब दिव्य होते हैं, चाहे बाह्य प्रतीति में वे हमें कैसे भी क्यों न लगते हों।
ivix
इस प्रकार तीसरा अध्याय 'कर्मयोग' समाप्त होता है।
चौथा अध्याय
I.अवतार-तत्त्व की सम्भावना, उसका उद्देश्य और उसकी प्रक्रिया
श्रीभगवान् उवाच
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ।। १।।
१. श्रीभगवान् ने कहाः मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान् को दिया था; विवस्वान् ने मनु (मनुष्यों के पिता) को दिया, मनु ने (सूर्यवंश के मुखिया) इक्ष्वाकु को दिया।
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ।। २॥
२. हे परंतप! इस प्रकार परंपरा से एक से दूसरे को प्राप्त होते हुए इस योग को राजऋषियों ने तब तक जाना जब तक कि यह योग दीर्घकाल बीतते-बीतते इस जगत् से लुप्त ही न हो गया।
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ।। ३।।
३. यही प्राचीन और आदिम योग जो कि सर्वोत्तम रहस्य है, आज मेरे द्वारा तुझे कहा गया है क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है।
जिस योग में कर्म और ज्ञान एक हो जाते हैं, कर्मयज्ञयोग ज्ञानयोग के साथ एक हो जाता है, जिस योग में कर्म की परिपूर्णता ज्ञान में होती है और ज्ञान कर्म को अवलंबन प्रदान करता है, उसका स्वरूप बदल देता है और उसे आलोकित कर देता है और फिर ज्ञान और कर्म दोनों ही उन परम भगवान् पुरुषोत्तम को समर्पित किये जाते हैं जो हमारे अन्दर नारायण-रूप से अभिव्यक्त होते हैं, जो नित्य हमारे हृदयों में गुप्त भाव से विराजमान हमारी संपूर्ण सत्ता व कर्म के ईश्वर हैं, जो मानव आकार में भी अवतार के रूप में, अर्थात् हमारी मानवीयता को अधिकृत करने वाले दिव्य जन्म में, प्रकट होते हैं, उस योग का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण बातों-बातों में यह कह गये कि यही वह पुरातन आदियोग है जो उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान् को प्रदान किया और विवस्वान् ने जिसे मनुष्यों के जनक मनु को और मनु ने सूर्यवंश के आदिपुरुष इक्ष्वाकु को दिया और इस प्रकार यह योग एक राजर्षि से दूसरे राजर्षि को मिलता रहा और इसकी परंपरा चलती रही जब तक कि फिर काल की गति में यह खो ही न गया। आज वही योग भगवान् अर्जुन को पुनः दे रहे हैं, क्योंकि वह अवतार श्रीकृष्ण का प्रेमी, भक्त, सखा और साथी है। क्योंकि भगवान् कहते हैं कि यह परम रहस्य है, - और ऐसा कहकर अन्य सब योगों से इसकी श्रेष्ठता दृढ़तापूर्वक बताते हैं, क्योंकि वे अन्य योग या तो निर्गुण ब्रह्म तक या सगुण साकार इष्टदेव तक ही ले जाने वाले हैं, या निष्कर्म ज्ञानस्वरूप मोक्ष अथवा आनन्द निमग्न मुक्ति तक ले जाने वाले हैं, जबकि यह योग परम रहस्य और संपूर्ण रहस्य उद्घाटित कर देता है; यह हमें दिव्य शांति और दिव्य कर्म को प्राप्त करानेवाला तथा पूर्ण स्वतंत्रता में एकीकृत हुए दिव्य ज्ञान, कर्म और परमानन्द को देनेवाला है। जिस प्रकार भगवान् की परम सत्ता अपनी अभिव्यक्त सत्ता के सभी भिन्न और यहाँ तक कि परस्पर विरोधी शक्तियों और तत्त्वों का समन्वय कर उन्हें अपने अन्दर एक कर लेती है वैसे ही यह योग सभी योगमार्गों को अपने-आप में एकीभूत कर लेता है। इसलिए गीता का यह योग केवल कर्मयोग नहीं है जैसा कि कुछ लोगों का आग्रह है और जिनके अनुसार यह तीनों मार्गों में से सबसे कनिष्ठ मार्ग है, अपितु यह परम योग है, जो पूर्ण समन्वयात्मक और अखंड है जो हमारी सत्ता की सभी शक्तियों को भगवन्मुखी बना देता है।
यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान् ने बातों-बातों में यह कह दिया है कि यह एक विशेष योग है और सर्वोत्तम रहस्य है। इसके बारे में अर्जुन को बताते हुए वे कहते हैं कि यह योग लुप्त हो गया था और इसके बारे में ऋषियों को भी पता नहीं था। आरम्भ में 'मैंने' अर्थात् स्वयं भगवान् ने इसे सूर्यदेव को बताया था, उनके द्वारा फिर सूर्य पुत्र मनु को यह प्राप्त हुआ, मनु से फिर इक्ष्वाकु को - जो कि सूर्यवंश के मुखिया थे और उसके बाद में ऋषियों-मुनियों को यह प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह योग बहुत लम्बे समय तक चलता रहा। परंतु धीरे-धीरे काल की गति में यह इस जगत् से लुप्त हो गया। भगवान् कहते हैं, 'परन्तु अब मैं इस योग के बारे में तुझे दुबारा बतला रहा हूँ जो कि बड़ा ही उत्तम रहस्य है।' इस योग को उत्तम रहस्य क्यों बताया गया है? इसके बारे में श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि क्योंकि यह ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति कर्म से आरम्भ करता है, परंतु कर्म के साथ-साथ ज्ञान भी चलता है, और इस प्रकार एक दूसरे को परिपूर्ण करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार कोई कर्म करता है। परंतु यदि वह कर्म उसने बहुत सच्चाई के साथ, भावना के साथ, यज्ञ के रूप में करने का प्रयत्न किया है, तो उसकी समझ में अभिवृद्धि होगी। अभिवृद्धि के कारण अब उसे और अधिक समझ में आने लगेगा। और इसके कारण कर्म पहले से बेहतर रूप से होने लगेंगे। और ज्यों-ज्यों वे बेहतर होते जाएँगे त्यों-ही-त्यों समझ में भी अभिवृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार ये परस्पर अभिवर्धित करते चलेंगे। साथ ही, सच्चा कर्मयोग सच्चे ज्ञानयोग से अभिन्न है। जो इन्हें भिन्न-भिन्न मानते हैं वे मूढ़ हैं। क्योंकि बिना पूर्ण रूप से ज्ञान हुए सच्चे रूप से कर्म हो ही नहीं सकते और इसीलिए बिना ज्ञान के कर्मयोग तो सिद्ध हो ही नहीं सकता। ऊपरी दृष्टि से ही ये भिन्न प्रतीत होते हैं पर वास्तव में तो दोनों आपस में गुँथे हुए हैं, अभिन्न हैं और साथ-साथ ही चलते हैं, और एक-दूसरे के परिपूरक हैं। आरम्भ में गीता इसी का समन्वय साधती है। इसलिये भगवान् ने इसे बहुत उत्तम रहस्य बताया है। इस समन्वय का भान न होने के कारण ही कुछ मनुष्य मूर्खतावश अपने को केवल सांख्ययोगी कहेंगे, जबकि अन्य दूसरे स्वयं को कर्मयोगी बताएँगे, परंतु वास्तव में तो किसी एक के बिना दूसरा अधूरा ही है। बिना कर्मयोग के सांख्ययोगी की अभिवृद्धि नहीं हो सकती, और यदि अभिवृद्धि हो भी जाए तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में वह कितनी सही है। हो सकता है कि वह अपनी ही भ्रांतियों में, अपने मन की निर्मित संरचनाओं में ही रहने लग जाये। वहीं, जो कर्मयोगी केवल कर्म से ही सरोकार रखता है और ज्ञान की उपेक्षा कर देता है, वह अपने अंदर मानो एक अवरोध पैदा कर लेता है क्योंकि सच्चा ज्ञान नहीं होने के कारण वह कर्म को यन्त्रवत् ही करता रहेगा, इसलिए ऐसे में सच्चा कर्म भी नहीं हो सकता। वह तो केवल अपने-आप को धोखा ही देता रहेगा। इस प्रकार एक-दूसरे को साथ में लेकर चले बिना दोनों में से कोई भी अपने-आप में संसिद्ध नहीं हो सकता। जब ये दोनों साथ-साथ चलेंगे तभी सच्ची क्रिया संसिद्ध हो सकती है।
आरम्भ के छः अध्यायों में गीता इसी समन्वय को साधने का कार्य करती है। केवल छठे अध्याय के अन्त में भगवान् कहते हैं कि यों तो सभी योगी श्रेष्ठ हैं परंतु उन सभी योगियों में भी मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है। तब ज्ञान और कर्म में एक नए तत्व-भक्ति -का भी समावेश करा दिया जाता है। इस तत्त्व पर बल देते हुए गीता बाद में इसका निरूपण करती है कि भक्ति ही सर्वोच्च तत्त्व है। और बिना भक्ति के भगवान् को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि केवल ज्ञान और कर्म को लेकर चलने पर एक सीमा के बाद वे रुक जाएँगे। और बिना भक्ति के सच्चा कर्म हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञान के आधार पर एक सीमा तक ही कर्मों को किया जा सकता है। जब तक उनमें भक्ति का समावेश नहीं होता, भक्ति का अवलंब प्राप्त नहीं होता तब तक योगक्रम आगे नहीं बढ़ सकता।
यदि व्यक्ति के अन्दर भगवान् के प्रति भाव नहीं है तो कर्म करना बड़ा कठिन हो जाएगा और ऐसे में तो कर्म एक बड़ी भारी यंत्रणा बन जाएगा, पीड़ा बन जाएगा। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तब उसके निमित्त कार्य करने में, उसकी सेवा करने में उसे जरा भी असुविधा, तकलीफ या कठिनाई अनुभव नहीं होती। उस प्रेम के कारण व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए कार्य किये बिना रह ही नहीं सकता। वहीं यदि वह भाव न हो तब फिर कर्म में अन्यमनस्कता आने लगती है, कर्म में सहज आनंद की बजाय बाध्यता का या फिर दबाव का अनुभव होने लगता है। ऐसे में यदि व्यक्ति को सेवा करने को कहा जाए तो उसके मन में अनेक तरीके के भाव उठ खड़े होते हैं जैसे कि 'सेवा करते हुए तो हम सुबह से नहा भी नहीं पाए हैं, रात भर सो भी नहीं पाए हैं, इसके कारण कुछ आवश्यक कार्य में भी व्यवधान आ गया है, आदि-आदि' और फिर अंततः यह कि 'यह करने से भी क्या लाभ है'। इस तरीके की बातें व्यक्ति के मन में आने लगती हैं। यदि किसी से आसक्ति हो तब तो सारा भाव, सारे क्रियाकलाप ही बदल जाते हैं। और वहीं यदि व्यक्ति को गहरा प्रेम हो तब तो सब कुछ ही बदल जाता है। व्यक्ति को यदि किसी से लगाव हो, तो भी उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, जैसे कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए या फिर कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए या भाई अपनी बहन के लिए इस तरीके की बात सोचेंगे भी नहीं कि उनकी सेवा करने के कारण वे सो नहीं पाए, या फिर उनका इसमें क्या लाभ। यदि लगाव हो, संबंध हो, प्रेम हो तो फिर ऐसे भाव तो उठते ही नहीं हैं। इसी प्रकार भगवान् के प्रति भी बिना प्रेम का भाव आए साधना नहीं हो सकती। इसलिए गीता इस तत्त्व का समावेश करती है और इसे पूर्ण रूप से विकसित करने के बाद ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय साधती है। यही गीता का पूरा विकासक्रम है। ऐसी इसकी संरचना है।
गीता में यह पहले ही आ चुका है कि भगवान् अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश करते हैं। परंतु अर्जुन का प्रश्न यह था कि 'मैं निष्काम कर्म करूँ कैसे? क्योंकि यदि कर्म का उत्प्रेरण कामना से हो रहा हो तब तो कहा जा सकता है कि अमुक काम को करने से कामना की पूर्ति होगी जबकि अमुक काम को करने में कोई लाभ नहीं है इसलिए उसे नहीं करना चाहिए। अतः कामना के आधार पर तो यह निर्णय हो सकता है, परन्तु जब कर्म को कामना के द्वारा नहीं करना है तब यह निर्धारण कैसे हो कि कौन-सा कर्म करें और कौन-सा न करें? इसके समाधान के रूप में भगवान् यज्ञ रूप से कर्म करने का निर्देश करते हैं और कहते हैं कि शुरू में मेरी प्रसन्नता के निमित्त सभी कर्म करो। क्योंकि आरंभ में ही कर्म निष्काम नहीं होंगे। ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ेगा त्यों ही त्यों निष्काम कर्म बढ़ेगा। क्योंकि निष्काम कर्म तो उसकी परिणति ही तो है। इसलिए भगवान् कहते हैं कि 'मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करना शुरू कर।' तब अर्जुन पूछता है कि 'आप कौन हैं?' जिनके लिए उसे कर्म करने को कहा जा रहा है वह उनका स्वरूप जानना चाहता है। यदि व्यक्ति यह मानकर कर्म करे कि 'मैं अपने मित्र के लिये, उसकी प्रसन्नता के लिये कर्म कर रहा हूँ, तो यह तो एक व्यक्तिगत बात ही हुई, एक व्यक्तिगत समाधान ही हुआ। परन्तु चूँकि योग सभी के लिए है, अतः एक व्यक्तिगत समाधान के आधार पर सभी योग कैसे करेंगे, इसीलिये एक ऐसे तत्त्व का निरूपण चाहिये जिस तक सभी पहुँच सकते हों।
तब फिर इस बात को प्रकट करने के लिए कि भगवान् का स्वरूप क्या है, गीता श्रीकृष्ण के मुख से यह प्रकट करा देती है कि हजारों-लाखों वर्ष पहले यह योग उन्होंने ही सूर्यदेव को दिया था। तब अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि 'वे' तो उसके समकालीन युग में ही पैदा हुए हैं इसलिए वे लाखों वर्ष पूर्व उस योग को सूर्यदेव को कैसे दे सके।
अब भगवान् उसे अवतार के रहस्य आदि के विषय में और भक्ति के विषय में बतलाएँगे। इस प्रकार भक्तियोग का सारा आधार, उसकी सारी पृष्ठभूमि इसी अध्याय में तैयार हो जाएगी। इसके बाद बीच में योग-साधना आदि के कुछ अन्य विषयों पर प्रकाश डालने के बाद अन्त में भगवान् भक्ति पर ही सारा बल देते हैं। इस प्रकार यह गीता का विकासक्रम है।
पर यहाँ यह आवश्यक है कि भगवान् अर्जुन को यह प्रकट करें कि नारायण हैं कौन? यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जिसके बिना कोई भी साधना होती ही नहीं है। भारतीय संस्कृति ने इस बात पर बहुत बल देकर कहा है कि भगवान् के व्यक्तित्व की उपस्थिति के बिना साधना नहीं हो सकती, भले ही व्यक्ति कितना भी ध्यान और अभ्यास क्यों न कर ले, क्योंकि ये सभी चीजें बहुत ही सीमित हैं और इन पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के पास हजारों-हजार तरह की सूक्ष्म शक्तियाँ हो सकती हैं, उसे हजारों प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं परन्तु भगवान् के व्यक्तित्व की उपस्थिति के बिना उसे कोई सच्चा आधार प्राप्त नहीं होता। इसीलिए गुरु परंपरा को इतना अधिक महत्त्व दिया जाता रहा है। गुरु को नारायण मानकर व्यक्ति उनके द्वारा भगवान् को प्राप्त कर सकता है। भले ही स्वयं गुरु को अनुभव प्राप्त न हो तो भी शिष्य को तो उसकी आवश्यकतानुसार अवश्य ही अनुभव प्राप्त हो जाएँगे। इस तरह की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है, क्योंकि बिना भगवान् के व्यक्तित्व के संपर्क में आए व्यक्ति मार्ग पर आगे नहीं जा सकता। यहाँ गीता इसी से आरम्भ करती है। इस सारी पृष्ठभूमि से हमें यह समझ आ जाएगा कि वास्तव में गीता का विकास किस प्रकार चल रहा है।
अर्जुन उवाच
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।। ४ ।।
४. अर्जुन ने कहाः आपका जन्म तो अर्वाचीन (अभी हाल ही का) है, विवस्वान् (जो कि मनुष्यों में प्रथम उत्पन्न होनेवाला और सूर्यवंश का पूर्वज है) का जन्म बहुत पहले हो चुका है; आपने इस योग को उसे पहले कहा था इसे मैं कैसे समजूं?
इस योग के एक से दूसरे को सौंपे जाने के कथन को अर्जुन इसके अत्यंत स्थूल अर्थ में ग्रहण करता है - दूसरा भी अर्थ है जिसमें इस बात को लिया जा सकता 3 - 3m पूछता है कि सूर्यदेव जो जीव-सृष्टि में प्रथमोत्पन्नों में से एक हैं, जो सूर्यवंश के आदिपुरुष हैं, उन्होंने मनुष्यरूप श्रीकृष्ण से, जो केवल अभी (हाल ही में) जगत् में उत्पन्न हुए हैं, यह योग कैसे ग्रहण किया। इस प्रश्न का उत्तर श्रीकृष्ण वैसा नहीं देते जैसा उत्तर देने की हम उनसे आशा कर सकते थे, कि उन्होंने सम्पूर्ण ज्ञान के स्रोत भगवान् के रूप में ही यह ज्ञान (दिव्य शब्द) उन सूर्यदेव को दिया जो उन भगवान् के ही ज्ञान के स्वरूप हैं और जो समस्त अंतर्बाह्य प्रकाश के देनेवाले हैं... इसकी अपेक्षा उन्होंने अपनी प्रच्छन्न भगवत्ता को प्रकाशित करने के लिए अर्जुन द्वारा प्रदत्त इस सुअवसर को स्वीकार किया, यह एक ऐसा प्रकाशन या उद्घोषणा थी जिसकी भूमिका वे तभी तैयार कर चुके थे जब उन्होंने कर्म करते हुए भी कर्मों से न बँधने वाले कर्मी के रूप में स्वयं का दिव्य दृष्टांत प्रस्तुत किया था, परंतु जिस बात को उन्होंने अभी तक सर्वथा स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किया था। अब वे अपने-आपको स्पष्ट शब्दों में अवतार' घोषित करते हैं।
श्रीअरविन्द आगे इसे और अधिक विस्तार से स्पष्ट करेंगे। जब हम यह मानते हैं कि सर्वत्र प्रभु विद्यमान हैं, उनके अतिरिक्त कहीं भी और किसी दूसरी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, वे ही सभी जगह और सभी चीजों में अभिव्यक्त हो रहे हैं तब फिर यह अवतार तत्त्व क्या है? और फिर मनुष्यों में और अवतार में इतना अन्तर कैसे होता है? जहाँ साधारण मनुष्य प्रकृति की क्रियाओं में इतना अधिक फंसा हुआ रहता है वहीं मनातार अपनी स्वतंत्र इच्छा-शक्ति से प्रकृति को कैसे प्रयोग में ला पाता है? यह कैसी व्यवस्था है?
----------------------------
...आधुनिक मन के लिए अवतार-तत्त्व तर्कबद्ध मानव-चेतना पर पूर्व की ओर से अंतर्प्रवाहित होनेवाले विचारों में से स्वीकार करने या समझने में सबसे अधिक दुःसाध्य विचार है। यदि अच्छे से अच्छे रूप में ले तो यह (तर्कबद्ध मानव-चेतना) अवतारतत्त्व को मानव शक्ति का, चरित्र का, प्रतिभा का, जगत् के लिए अथवा जगत् में की गई किसी महान् अभिव्यक्ति का महज एक रूपक मानती है, और यदि संकीर्णतम भाव से ग्रहण करे तो इसे महज एक अंधविश्वास मानती है, एक काफिर या नास्तिक के लिए यह एक मूर्खता है और यूनानियों के लिये मार्ग का रोड़ा है। जड़वादी तो इस विचार की ओर देख भी नहीं सकता, क्योंकि वह ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानता; तर्कवादी या देवतावादी (जो मानता है कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना कर इसे छोड़ दिया और जो ईश्वर के प्राकट्य को स्वीकार नहीं करता) के लिए यह मूर्खता और उपहास का विषय है; पक्के द्वैतवादी के लिए, जो मानव और दिव्य प्रकृति के बीच न मिट सकने वाला अंतर देखता है, यह ईश्वर-निन्दा का आभास देता है। तर्कवादी का पक्ष है कि यदि ईश्वर विद्यमान है तो वह विश्वातीत या अतिवैश्विक है और संसार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, अपितु उन्हें एक सुनिश्चित विधान के तंत्र द्वारा चालित होने देता है, - वस्तुतः एक प्रकार से वह विश्व से सुदूर कोई संवैधानिक राजा या कोई जड़वत् आध्यात्मिक राजा है, अधिक-से-अधिक वह प्रकृति की क्रिया के पीछे रहनेवाला, सांख्यों द्वारा वर्णित कोई व्यापक या अमूर्त साक्षी पुरुष के जैसा उदासीन अकर्ता आत्म-तत्त्व है; वह विशुद्ध आत्मा है और शरीर धारण नहीं कर सकता: वह अनन्त है और सीमित नहीं हो सकता जिस प्रकार मनुष्य सीमित है, वह चिर अजन्मा सृष्टिकर्ता है और संसार में उत्पन्न कोई प्राणी नहीं हो सकता, – ये बातें उसकी परम् निरपेक्ष सर्वशक्तिमत्ता के लिए भी असंभव हैं। इन सभी आपत्तियों में द्वैतवादी यह भी जोड़ देगा कि ईश्वर अपने व्यष्टिभाव में हैं परंतु उनका कार्य या भूमिका तथा उनकी प्रकृति मनुष्य से भिन्न और प पृथक् हैं; पूर्ण (भगवान् या पुरुष) मनुष्य की नहीं धारण कर सकता: अजन्मा साकार परमेश्वर मनुष्य व्यक्तित्व के रूप में नहीं उत्पन्न हो अपूर्णता को को अपने ऊपर सकताः सर्वलोकमहेश्वर प्रकृतिबद्ध मानव क्रिया में और एक नाशवान् मानव-शरीर में सीमित नहीं हो सकता। प्रतीत होता है कि तर्क या बुद्धि की प्रथम दृष्टि के लिए बड़े विकट ये आक्षेप गीता के श्रीगुरु की दृष्टि के सामने विद्यमान रहे होंगे जब वे कहते हैं कि, सद्यपि भगवान् अपनी आत्म-सत्ता में अज हैं, अव्यय हैं, भूतेश हैं, फिर भी वे अपनी प्रकृति का अधिष्ठान कर के अपनी माया के द्वारा जन्म ग्रहण करते हैं; और वे, जिन्हें मूढ़ व्यक्ति मनुष्य-शरीर में स्थित होने के कारण तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, अपनी परम सत्ता में। सबके स्वामी हैं... और गीता इन सभी विरोधों को शांत कर पाती है और इन सभी विरोधाभासों में समन्वय साधने में समर्थ होती है, क्योंकि यह अस्तित्व के, ईश्वर के और जगत् के विषय में वेदान्तिक दृष्टिकोण से आरम्भ करती है। क्योंकि वस्तुओं के वेदान्तिक दृष्टिकोण से ये सभी बाहर से दिखने में घोर आक्षेप आरम्भ से ही निस्सार और निरर्थक हैं। वेदान्त की योजना के लिए वस्तुतः अवतार का विचार अनिवार्य नहीं है, परंतु फिर भी एक सर्वथा युक्तिसंगत और न्यायसंगत धारणा के रूप में यह विचार स्वभावतया ही इसमें आ जाता है।
इसमें श्रीअरविन्द गीता के ही उन श्लोकों को लेकर भेद बताते हैं जिनमें भगवान् सामान्य जीव के जन्म ग्रहण में और स्वयं अपने अवतार रूप से जन्म ग्रहण में भेद करते हैं। सामान्य सृष्टि रचना में भगवान् अपने गुणों और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के अधीन हो जाते हैं और उससे धोरे-धीरे विकसित होते रहते हैं। परंतु जब वे स्वयं अवतार लेते हैं तब प्रकृति का अधिष्ठान कर के आविर्भूत होते हैं। इसमें भगवान् कहते हैं कि प्रकृति के गुण और स्वभाव तो वैसे ही रहते हैं परन्तु उनका उपयोग वे स्वतंत्र रूप से स्वेच्छापूर्वक अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपने दृष्टिकोण से करते हैं। इसमें वे प्रकृति के वशीभूत नहीं होते। ऊपरी प्रकृति में चाहे वश्यता दिखाई दे सकती है पर वास्तव में अवतार वशीभूत नहीं होते। यह एक बड़ा ही सूक्ष्म भेद है। जीव प्रकृति के वशीभूत होता है जबकि अवतार प्रकृति के वशीभूत न होकर उस पर अधिष्ठित होते हैं। वे हमें वशीभूत प्रतीत हो सकते हैं पर ऐसा तो ऊपरी दिखावा मात्र है, वास्तव में वे वशीभूत नहीं अपितु पूर्णतः स्वतंत्र होते है क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हालाँकि भगवान् की विभूति के अंदर उनका विशेष प्रकाश होता है, और उसे प्रकृति के विधान में स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, पर वह स्वतंत्रता प्रकृति के विधान के अंदर ही है। और विभूति को इस संबंध में ज्ञान हो यह भी आवश्यक नहीं है। अवतार में अंतर यह है कि वे अपने स्वरूप के विषय में सचेतन होते हैं। और वे प्रकृति को अपने वश में रखकर क्रिया करते हैं। प्रकृति को वे अपनी इच्छा या आवश्यकतानुसार प्रयोग करते हैं। उनकी इस क्रिया को हम चमत्कार या अन्य कोई भी नाम दे सकते हैं। जीव और अवतार में यही अन्तर है। आगे अवतार विषय पर और अधिक गहराई से चर्चा आएगी।
------------------
क्योंकि यहाँ सभी कुछ ईश्वर है, आत्मा या स्वयं-सत् अथवा एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म है, - इसके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है, इससे अलग तथा इससे भिन्न कुछ नहीं है और इसके अतिरिक्त और कोई चीज हो ही नहीं सकती जो उससे अलग और भिन्न हो; प्रकृति भागवत् चेतना की ही एक शक्ति होने के अतिरिक्त न कुछ और है न हो सकती है; सभी प्राणी एक ही भागवत् सत्ता के आन्तर और बाह्य, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, जीवरूप और देहरूप के अतिरिक्त न कुछ हैं न हो सकते हैं, जो कि उसी भागवत् चेतना की शक्ति से उत्पन्न होते और उसी में स्थित रहते हैं। अनंत सत्ता सीमितता धारण करने में असमर्थ हो यह तो दूर रहा, अपितु संपूर्ण ब्रह्माण्ड उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं; इस समग्र विशाल जगत् में, जहाँ हम रहते हैं, हम जिधर दृष्टि उठाकर देखें, चाहे जैसे देखें, उसी को देख सकते हैं। आत्मा का साकार न हो सकना अथवा स्वयं को अन्नमय या मनोमय रूप के साथ सम्बन्ध जोड़ने और एक परिसीमित प्रकृति या शरीर धारण करने से घृणा करना तो दूर रहा, यहाँ तो जो कुछ है वही है, जगत् का अस्तित्व हो उसी के सम्बन्ध से, उसी के द्वारा परिसीमित प्रकृति और शरीर को धारण किये जाने के कारण है।
अजन्मा जन्म ग्रहण कर सकने में असमर्थ हो यह बात तो दूर रही, यहाँ तो प्रत्येक जीव अपने व्यष्टिभाव में रहते हुए भी वही अजन्मा आत्मा है, वही सनातन अनादि अनंत है और अपने सारभूत अस्तित्व और अपनी सार्वभौमिकता में सभी जीव वही एक अजन्मा आत्मा हैं जिसकी जन्म और मृत्यु केवल आकार-ग्रहण और आकार-परिवर्तन रूपी घटनाएँ मात्र हैं। पूर्ण द्वारा अपूर्णता को धारण किये जाना ही इस जगत् का संपूर्ण गुह्य विषय है; परंतु यह अपूर्णता धारण किए गये मन अथवा शरीर के रूप और कर्म में ही प्रकट होती है, यहाँ के बाह्य दृश्य जगत् में ही रहती है, - जो इसे धारण करता है, उसमें अपने-आप में कोई अपूर्णता नहीं होती; वैसे ही जैसे सूर्य, जो सबको आलोकित करता है, उसमें प्रकाश या दर्शन-शक्ति का कोई दोष नहीं होता, कमी होती है केवल व्यक्तिगत दर्शनेन्द्रिय की क्षमता में। और न ही ऐसा है कि भगवान् किसी सुदूर स्वर्ग में विराजे इस जगत् पर शासन करते हों, अपितु यह शासन वे अंतरंग सर्वव्यापकता से करते हैं; शक्ति की प्रत्येक सीमित क्रिया अनन्त शक्ति की ही क्रिया होती है, न कि अपने ही बल पर परिश्रम करती किसी सीमित पृथक् स्वयंभू क्रिया-शक्ति की क्रियाः संकल्प और ज्ञान की प्रत्येक सीमित क्रिया में हम उसे आश्रय प्रदान करती अनंत सर्व-संकल्प और सर्व-ज्ञान की किसी क्रिया को खोज सकते हैं।... इसलिए अवतार-तत्त्व की सम्भावना के विरुद्ध हमारी तर्क-बुद्धि द्वारा प्रस्तुत कोई भी आपत्तियाँ सिद्धान्ततः टिक नहीं सकतीं; क्योंकि यह बौद्धिक तर्क द्वारा उपस्थित एक ऐसा व्यर्थ का विभेद है जिसे संपूर्ण दृश्य-जगत् और जगत् की सारी वास्तविकता दोनों ही प्रतिक्षण खंडित और अप्रमाणित सिद्ध कर रहे हैं।
श्रीभगवान् उवाच
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ।। |4|
५. श्रीभगवान् ने कहाः हे अर्जुन ! मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं और तेरे भी बीत चुके हैं; उन सबको मैं जानता हूँ किन्तु हे परन्तप, तू नहीं जानता।
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ।। ६।।
६. यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, यद्यपि मैं अपनी आत्म-सत्ता में अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त भूतों का ईश्वर हूँ, तथापि मैं अपनी प्रकृति के ऊपर अधिष्ठित होकर अपनी माया के द्वारा जन्म ग्रहण करता हूँ।
अब यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा के एक हल्के से किन्तु फिर भी बड़े महत्त्वपूर्ण अंतर से गीता, समान ही रीति से, प्राणियों के सामान्य जन्म और एक अवतार के रूप में स्वयं के जन्म ग्रहण में भगवान् की क्रिया का वर्णन करती है। "अपनी प्रकृति को वश में कर के, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य," यह बाद में कहेगी, "मैं इन प्राणियों के समूह को जो प्रकृति के वश में हैं अवशं प्रकृतेर्वशात्, उत्पन्न करता हूँ, विसृजामि।" और यहाँ कहते हैं कि, "अपनी प्रकृति के ऊपर अधिष्ठित होकर मैं अपनी स्वयं की माया से जन्म लेता हूँ, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय... आत्ममायया, मैं अपने-आपको उत्पन्न करता हूँ, आत्मानम् सृजामि।" अवष्टभ्य शब्द से जो क्रिया अभिप्रेत है वह एक नीचे की ओर सशक्त दबाव है जिसके द्वारा वशीभूत पदार्थ को उसकी गति और उसकी क्रिया में वशीकृत (overcome), अनुबाधित (oppressed), अवरुद्ध (blocked) या परिसीमित (limited) किया जाता है जिसमें वशीभूत व्यक्ति या पदार्थ अवश रूप से नियामक सत्ता (वशी) के वश में होता है अवशं वशात्; इस क्रिया में प्रकृति जड़-यंत्रवत् बन जाती है और इसके प्राणीसमूह उसकी इस यांत्रिकता में बेबस वशीभूत रहते हैं, न कि स्वयं अपने कर्म के स्वामी होते हैं। इसके विपरीत 'अधिष्ठाय' शब्द में जो क्रिया (भाव) निहित है वह है 'के अन्दर स्थित होना या निवास करना', परंतु साथ ही यह 'प्रकृति के ऊपर और परे स्थित होना' भी सूचित करता है, अर्थात् अंतर्यामी भगवान्, अधिष्ठातृ-देवता, द्वारा एक सचेतन नियंत्रण और शासन, जिसमें पुरुष अज्ञान में प्रकृति द्वारा विवश रूप से नहीं चालित होता, अपितु प्रकृति पुरुष के प्रकाश और संकल्प से परिपूर्ण होती है।...
ix.8
अतः गीता की भाषा स्पष्टतः यह दर्शाती है कि दिव्य जन्म हमारी मानवीयता में चेतन भगवान् का जन्म है और यह मूलतः सामान्य जन्म का विपरीत है भले ही (दोनों स्थितियों में) जन्मग्रहण में एक ही जैसे साधनों को प्रयोग में लाया जाता है- क्योंकि यह अज्ञान में जन्म नहीं होता, अपितु यह सज्ञान जन्म होता है, कोई भौतिक घटना नहीं अपितु यह आत्मा का जन्म है।... सामान्य मानव-जन्म में मानवरूप धारण करनेवाले विश्वेश्वर का प्रकृतिभाव ही प्रमुख होता है; अवतार के मानव-जन्म में उनका ईश्वरभाव प्रमुख होता है। एक में ईश्वर मानव-प्रकृति को अपनी आंशिक सत्ता पर अधिकार जमा कर उस पर हावी होने देते हैं; जबकि दूसरे में वे अपनी अंशसत्ता और उसकी प्रकृति को अपने अधिकार में लेकर उस पर दिव्य रूप से शासन करते हैं। गीता हमें बतलाती प्रतीत होती है कि साधारण मनुष्य के समान क्रमविकास के द्वारा या आरोहण के द्वारा, अथवा दिव्य जन्म में विकास के द्वारा यह (अवतार-तत्त्व) साधित नहीं होता, अपितु भगवान् द्वारा मानवीयता के उपादान में सीधे अवतरण कर के उसके स्वभाव को धारण करने से होता है... अतः अवतार है दिव्य आत्मा श्रीकृष्ण द्वारा सत्ता की उस दिव्य स्थिति की मानवता के अन्दर सीधी अभिव्यक्ति, जिस स्थिति तक ऊपर उठने के लिए मानव-आत्मा, श्रेष्ठतम मानव प्रतिरूप, विभूति रूप अर्जुन को श्रीगुरु द्वारा निमंत्रित किया जाता है, और जिस स्थिति तक वह अपनी सामान्य मानवता की अज्ञानता और सीमितता को पार कर के ही उठ सकता है। यह ऊपर से उसी तत्त्व की नीचे आकर अभिव्यक्ति है जिसे हमें नीचे से ऊपर की ओर विकसित करना होगा; यह मानव-सत्ता के उस दिव्य जन्म में भगवान् का अवतरण है जिसमें हम मर्त्य प्राणियों को आरोहण करना है; यह मानव-प्राणी के सम्मुख, मनुष्य के ही आकार और प्रकार के अन्दर तथा मानव जीवन के सिद्ध आदर्श प्रमाण के अन्दर, भगवान् का एक आकर्षक दिव्य उदाहरण है।
इसमें भगवान् ने सामान्य मानवों के जन्म और स्वयं अपने जन्म ग्रहण के बीच के भेद को बता दिया है। सामान्य सृष्टि के निर्माण में भगवान् अपनी प्रकृति के वश में कर के जीवों को उत्पन्न करते हैं। परंतु स्वयं अपने जन्म ग्रहण में भगवान् प्रकृति के वश में न होकर उस पर अधिष्ठित होते हुए निज माया से अपने-आप को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जन्म ग्रहण में भगवान् की निज प्रकृति या परा प्रकृति, जो कि स्वयं जगदम्बा हैं, के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। कोई भी मनुष्य, कितने भी आरोहण से, कितनी भी साधना से, कितने भी प्रकाश से उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वह तो अनंत है जबकि यह तो सीधा अवरोहण है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। इसलिए यह एक भिन्न प्रक्रिया है। इसीलिए श्रीरामकृष्णजी जीव-कोटि और ईश्वर-कोटि के बीच भेद करते थे। वे स्वामी विवेकानन्द को ईश्वर-कोटि बताते थे। यह एक बड़ी विलक्षण बात है। और हमारी संस्कृति में तो सारा भागवत् धर्म इसी पर आधारित है। भागवत् इसका और भी विशिष्ट रूप से वर्णन करती है कि जो सत्ता मनुष्य शरीर धारण करती है वह कोई सामान्य सत्ता नहीं है। जिन परम पुरुष पुरुषोत्तम से असंख्यों ब्रह्माण्ड बनते हैं, वे ही स्वयं शरीर धारण करते हैं। यह बड़ी ही विलक्षण बात है। इसलिए इसका कोई ओर-छोर नहीं है। इसीलिए एक भजन में कहते हैं कि 'निराकार ब्रह्म रह्यो गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार, कौन पावे याको पार।' इसी प्रकार, जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देना चाहते थे तो गोपियों ने कहा कि 'हमें साधना से, ज्ञान प्राप्त कर के विष्णु का अनुभव प्राप्त करने से क्या तात्पर्य, इस तरीके की बातें आप हमें क्यों समझाते हैं, हमारा तो श्रीकृष्ण से सतत् ही संपर्क है।' और उस सतत् संपर्क से व्यक्ति की आत्मा में जो क्रिया होती है उसका तो कोई अन्त ही नहीं है।
इसी चीज को श्रीअरविन्द ने अपने आश्रम में व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित किया। वहाँ जब जगदम्बा स्वयं सशरीर मौजूद थीं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जब एक बार व्यक्ति उनके साथ संपर्क में आ जाता है तब फिर साधना करने की बात तो बिल्कुल निरर्थक है। इसकी बजाय कोई भी समझदार व्यक्ति यही चाहेगा कि वह श्रीमाँ की निजी सेवा करने का परम सौभाग्य पा सके, उनका कोई सेवाकार्य कर सके। अन्य कोई चीज से तो उसे कोई सरोकार ही नहीं होगा। यही वास्तविकता है कि श्रीमाँ के संपर्क में आने मात्र से सब साधना हो जाती है। परन्तु जो व्यक्ति इन सब चीजों को नहीं समझ सकता वह तो यही कहेगा कि आश्रम में तो लोगों से साधना करवानी चाहिए जबकि यहाँ तो कोई कसीदा कर रहा है, कोई श्रीमाँ के लिए साड़ी बना रहा है, कोई अन्य कुछ कर रहा है। और फिर सभी लोग श्रीमाँ को प्रणाम करने में ही बहुत सा समय बिताते हैं। यहाँ तो सब लोग इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। इन्हें तो साधना से कोई लेना-देना ही नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति इन सब बातों को कैसे समझ सकता है कि साधना का सार ही इन्हीं चीजों को करने में है। और वास्तव में यह तत्त्व ऐसा है कि यदि व्यक्ति इसे एक बार देख ले तो उसे अनुभव होगा कि दूसरी और कोई चीज करने में तो सार ही नहीं है। और जहाँ श्रीमाँ व श्रीअरविन्द स्वयं मौजूद हैं वहाँ का सारा वातावरण तो दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो उठता है। अन्यथा तो व्यक्ति अपने निजी प्रयास से बड़ी कठिनाई से साधना करता है, उसके बल पर उसे कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, तब फिर ब्रह्म का अनुभव होता है, आदि-आदि। परंतु यहाँ तो बात ही दूसरी है। जैसे कि, उद्धव जी जब गोपियों को ब्रह्मज्ञान देने गए तब उनसे मिलने पर उन्हें समझ आ गया कि भगवान् ने उन्हें ब्रह्मज्ञान देने के लिए नहीं अपितु स्वयं यह समझने के लिए उनके पास भेजा है कि ज्ञान के भ्रम की इस मूर्खता से वे कैसे बाहर निकलें। जब उद्धव जी ने गोपियों को ब्रह्म के चिंतन आदि का ज्ञान देना चाहा तो गोपियों ने कहा 'ऊधो मन न भये दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ अवराधे ईस'। अर्थात् 'हमारे पास तो एक ही मन था और वह तो श्याम के साथ चला गया, इसलिए अब दूसरा मन है नहीं जो तुम्हारे ब्रह्म में हम लगा सकें।' उसी प्रकार जो सच्चे भाव से श्रीमाँ की सेवा में आ गया हो उसे यदि कहा जाए कि तू भगवान् की अनुभूति या साक्षात्कार कर, तो वह यही कहेगा कि उसके पास तो उस सब के लिए फुरसत ही नहीं है।
यह कोई अतार्किक नहीं बल्कि बहुत ही व्यावहारिक बात है। यह अवतार तत्त्व बहुत शक्तिशाली है। जब व्यक्ति गुरु के रूप में, विभूति के रूप में उनकी सेवा करता है, उनसे संपर्क साधता है, उनकी पूजा करता है तभी उसका निस्तारा हो सकता है, अन्य किसी साधना से वास्तव में कुछ नहीं हो सकता। जब गीता में अर्जुन ने भगवान् से पूछा कि वह कौन-सा मार्ग अपनाए तब भगवान् ने बड़ी ही स्पष्टता से कह दिया कि "जो लोग अपनी समस्त इन्द्रियों को संयत कर के, सर्वत्र समदृष्टि होकर अक्षर, अनिर्देश्य की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं परंतु जो लोग अपने मन को मुझमें प्रतिष्ठित करते हैं और परम श्रद्धा से युक्त, निरंतर मेरे साथ युक्त रहते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं सर्वाधिक पूर्णता से योग में युक्त मानता हूँ।" हालाँकि जो अक्षर ब्रहा की साधना करते हैं वे अपने लक्ष्य में गलत नहीं हैं, परन्तु वे एक अधिक कठिन तथा कम पूर्ण और कम सिद्ध मार्ग का अनुसरण करते हैं।
xii. 3-4
इसलिए भगवान् की व्यक्तिगत उपस्थिति का बड़ा भारी महत्त्व है। गीता का अर्जुन को परम् वाक्य भी यही है कि 'किसी साधना आदि की आवश्यकता नहीं है, तू तो बस मेरी शरण में आ जा।' भगवान् ने पहले तो अर्जुन से कहा कि ईश्वर सभी भूतों के हृदय में स्थित हैं और अपनी माया से यंत्र के रूप में सबको घुमाते हैं, तू उन्हीं की शरण ग्रहण कर जिससे कि तुझे परा शांति और शाश्वत पद प्राप्त होगा। परंतु बाद में वे उसे सर्वगुह्यतम् बात कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़ कर मेरी शरण में आ जा। इस प्रकार गीता में भी भगवान् की व्यक्तिगत उपस्थिति की परम् महत्ता पर बल दिया गया है।
श्रीअरविन्द आश्रम का संपूर्ण आधार भी यही है। इसलिए यदि हम श्रीमाँ के निमित्त, उनके प्रति भावना से कार्य करते हैं तो हमें साधना से कोई विशेष तात्पर्य नहीं है। साधना तो अहंकारमय है। साधना में तो व्यक्ति को स्वयं के ऊपर केन्द्रित होना पड़ता है क्योंकि वह निजी सामर्थ्य के आधार पर सोचता है कि उसे अमुक प्रयास करने हैं, ध्यान आदि की अमुक क्रियाएँ करनी हैं। इसीलिए भागवत् कहती है कि ब्रह्म की अनुभूति, मुक्ति, ब्रह्म का ज्ञान आदि सब तो सात्त्विक बातें हैं, परन्तु मुकुन्द की सेवा, या हम कह सकते हैं कि श्रीमाँ की सेवा, निस्त्रैगुण्य है। साधना आदि के अंदर तो व्यक्ति उसी फंदे में पड़ा रहता है। फंदे से तो व्यक्ति तभी निकल सकता है जब भगवान् के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ उसका भौतिक संसर्ग होगा। इसके बिना वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। इस सत्य को भगवान् अनेक बार सामने लाएँगे। गीता का सार भी यही है। इसमें जब अर्जुन पूछता है कि 'मुझे यह युद्ध क्यों करना चाहिए', तब भगवान् उसे समझाते हैं कि ऐसा उसे किसी सिद्धांत के कारण या किसी मत के कारण, या किसी ब्रह्मज्ञान के कारण नहीं अपितु इस कारण करना है क्योंकि ऐसी उनकी इच्छा है। यही तो गीता का उत्तर है कि यह परिणाम मेरे द्वारा नियत-निर्धारित है, तू तो केवल निमित्तमात्र बन जा।
प्रश्न : क्या भगवान् श्रीराम को यह पता था कि वे अवतार हैं?
उत्तर : श्रीअरविन्द के अनुसार तो वे जानते थे कि वे अवतार हैं परन्तु उन्होंने ऐसा प्रकट नहीं किया। प्रकट तो कोई करता भी नहीं है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि भगवान् को कोई गुह्य ज्ञान हो। जब शबरी ने उन्हें बताया कि 'मेरे गुरुजी पहले ही आपके आगमन के बारे में बता गए थे', तब भगवान् श्रीराम ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि उन्हें तो पहले से इस बात का पता ही नहीं था। इसलिए, आवश्यक नहीं है कि अवतार की सतही चेतना में उसे इस बात का भान हो। विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी जन्म से ही अपनी विशिष्टता का आभास हो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रीचैतन्य महाप्रभु का ही उदाहरण लें। वे तो जब आवेश आता था तभी अवतार भाव में जाते थे अन्यथा वे अपने को एक भक्त ही मानते थे। संन्यास से पूर्व तो वे अपने को एक सामान्य पंडित ही मानते थे। गीता की जो पद्धति है उसमें तो बात कुछ भिन्न है। उसके अनुसार तो अवतार अपनी योगमाया से स्वयं ही आविर्भूत होते हैं, उन्हें प्रकृति के तत्त्वों की आवश्यकता नहीं होती। परंतु स्वयं श्रीरामकृष्ण और श्रीअरविन्द को ही लें तो उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि वे अवतार हैं। श्रीअरविन्द तो अपने विषय में लिखते हैं कि उन्हें आरंभ में भगवान् की सत्ता मात्र में कोई विश्वास नहीं था। इस प्रकार उनकी सतही प्रकृति में तो उन्हें कुछ विशेष आभास नहीं था पर गहराई में कोई चीज ऐसी थी जो जानती थी। पर यह अंतर्निहित चीज जीवन काल में पहले आ सकती है, और यह बाद में भी आ सकती है। इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। इन चीजों के कोई बँधे-बँधाए नियस नहीं हैं। पर इतना अवश्य है कि अपने भीतर वह जानता है कि वह क्या है। इसी प्रकार श्रीमाताजी के स्वरूप के विषय में तो श्रीअरविन्द ने ही स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि वे स्वयं जगदम्बा हैं। चूंकि श्रीअरविन्द ने इस विषय पर इतना कुछ लिखा है इसलिए हम इस तत्त्व का कुछ अनुमान लगा सकते हैं अन्यथा केवल गीता में आए वर्णन से तो अवतार तत्त्व का बहुत सीमित ज्ञान ही होता है। श्रीअरविन्द ने तो श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीचैतन्य, श्रीरामकृष्ण, बुद्ध आदि विभिन्न अवतारों के संबंध में अपने पत्रों के माध्यम से अनेक रहस्यों को प्रकट किया है। और इस कारण उनकी कृपा से हमें इस तत्त्व के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।। ७।।
७. हे भारत! जब-जब धर्म क्षीण हो जाता है और अधर्म ऊपर को उठ जाता है (बढ़ जाता है) तब मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।।८।।
८. सत्पुरुषों के परित्राण के लिये, दुष्कर्म करनेवालों (दुष्टों) के विनाश के लिये, और धर्म की स्थापना करने के लिये मैं युग-युग में उत्पन्न होता हूँ।
...यहाँ हमें बड़ी सावधानीपूर्वक यह ध्यान देना होगा कि अवतार का अवतरण – जो कि मानवजाति के अन्दर अभिव्यक्त भगवान् का परम रहस्य है – केवल धर्म के संस्थापन के लिए ही नहीं होता; क्योंकि धर्मसंस्थापन अपने-आप में कोई सर्वथा पर्याप्त हेतु नहीं है, कोई ऐसा संभव परम् लक्ष्य नहीं है जो ईसा या कृष्ण या बुद्ध के आविर्भाव के लिए पर्याप्त हो, अपितु धर्मसंस्थापन तो किसी महत्तर उद्देश्य तथा एक अधिक परम् और दिव्य कार्यसिद्धि की एक सामान्य अवस्थामात्र है। कारण, दिव्य जन्म के दो पहलू होते हैं; एक है अवतरण, मानव जाति में भगवान् का जन्मग्रहण, मानव आकृति और प्रकृति में भगवान् का स्वयं को अभिव्यक्त करना, यह सनातन अवतार है; दूसरा है एक आरोहण, भगवत्ता में मनुष्य का जन्मग्रहण, दिव्य प्रकृति और चेतना में उसका उत्थान मद्भावमागतः; यह आत्मा के द्वितीय जन्म में सत्ता का नवजन्म है। यह नवजन्म ही है जिसकी चरितार्थता के लिए अवतार लेना और धर्मसंस्थापन करना अभिप्रेत होते हैं। गीता के अवतार विषयक सिद्धांत का यह द्विविध पहलू प्रायः ही उस सरसरी तौरपर पढ़ने वाले पाठक से छूट जाता है जो, अधिकांश पाठकों की तरह, इस ग्रंथ की गंभीर शिक्षा के एक सतही अर्थ को ग्रहण करने भर से ही संतुष्ट हो जाता है। और साथ ही सांप्रदायिक कठोरता में रूढ़ हुआ औपचारिक भाष्यकार भी इस पहलू से चूक जाता है। और फिर भी, निश्चय ही, इस सिद्धांत के संपूर्ण आशय को समझने के लिए इसे समझना आवश्यक है। अन्यथा अवतार का विचार केवल एक मतविशेष भर, एक प्रचलित अंधविश्वास भर रह जाएगा, या फिर ऐतिहासिक या पौराणिक अतिमानवों का काल्पनिक या रहस्यमय तरीके से देवत्वारोपण (deification) होगा, न कि वह होगा जो गीता अपनी संपूर्ण शिक्षा को बना देती है - एक गंभीर दार्शनिक और धार्मिक सत्य तथा सभी कुछ के परम् रहस्य, 'रहस्यं उत्तमं', को प्राप्त करने का एक आवश्यक अंग या उसकी ओर एक चरण।
यदि मानव का भगवत्ता में यह उत्थान मानवता के अंदर भगवान् के अवतरण के द्वारा सहायता प्राप्त न हो तो केवल धर्मसंस्थापन हेतु अवतार ग्रहण एक व्यर्थ विषय होगा क्योंकि केवल धर्म, न्याय या धर्माचरण के मानदण्डों को, किसी अवतार के वास्तविक अवतरण के बिना भी, दिव्य सर्वशक्तिमत्ता द्वारा सदा ही अपने सामान्य माध्यमों के द्वारा – महान् व्यक्तियों अथवा महान् गतियों या आंदोलनों द्वारा, साधु-संतों तथा राजाओं तथा धर्मगुरुओं के जीवन व कर्म के द्वारा भी बनाए रखा जा सकता है... अवतार-तत्त्व के विषय में यह दूसरा और वास्तविक उद्देश्य ही गीता के समग्र प्रतिपादन का सारतत्त्व है, यह बात इस श्लोक से ही, यदि इसका यथार्थ रूप से विचार किया जाए तो, प्रत्यक्ष है। परंतु इसे केवल अपने-आप में (एकांगी रूप से) लेकर ही नहीं - जो कि गीता के श्लोकों के साथ व्यवहार करने का सदा ही गलत तरीका होता है, अपितु अन्य श्लोकों के साथ उसके सही घनिष्ठ सम्बन्ध को तथा (गीता की) संपूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाए तो यह बात और भी अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। हमें गीता के सबमें एक ही आत्मा के सिद्धांत को, प्रत्येक प्राणी के हृदय-प्रदेश में भगवान् के विराजमान होने के सिद्धांत को, सृष्टिकर्ता और उनकी सृष्टि के बीच सम्बन्ध के विषय में इसकी शिक्षा को, इसके द्वारा विभूति-तत्त्व के विचार पर दिये जोरदार आग्रह को ध्यान में रखना होगा और इन सब को एक साथ विचारना होगा। साथ ही उस भाषा पर भी ध्यान देना होगा जिसमें भगवान् स्वयं अपने निष्काम कर्मों का दिव्य उदाहरण देते हैं, जो मानव श्रीकृष्ण पर उतना ही प्रयुक्त होता है जितना सर्वलोकमहेश्वर पर... और हमें इन विचारों के प्रकाश में इस प्रस्तुत संदर्भ का अभिप्राय निकालना होगा और (वैसे ही) इस उक्ति का अर्थ निकालना होगा कि उनके दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के विषय में ज्ञान द्वारा मनुष्य भगवान् के पास आते हैं और भगवान् से परिपूर्ण होकर तथा यहाँ तक कि भगवन्मय होकर तथा उनकी शरण ग्रहण कर के वे उनके स्वभाव और भाव, मद्भावम्, को प्राप्त होते हैं। क्योंकि, तब हम दिव्य जन्म और उसके हेतु को समझ सकेंगे, किसी अलग-थलग या एकाकी एवं चमत्कारपूर्ण घटना के रूप में नहीं, अपितु जगत्-अभिव्यक्ति की संपूर्ण योजना में उसके उचित स्थान के अनुसार समझ सकेंगे; बिना इसके हम अवतार के इस दिव्य रहस्य तक नहीं पहुँच सकते, और तब फिर या तो हम इस पर सर्वथा संदेह अथवा अविश्वास करेंगे या फिर, हो सकता है कि, इसे बिना समझे ही अंधश्रद्धा के कारण स्वीकार कर लेंगे अथवा इसके बारे में आधुनिक मन के उन क्षुद्र और बाहरी विचारों में जा फँसेंगे जिनसे इसका समस्त आंतरिक और लाभकारी अर्थ नष्ट हो जाता है।
iv.9-10
प्रश्न : विभूति तत्त्व का क्या अर्थ है?
उत्तर : गीता में विभूति योग के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो भी चीज विशिष्ट है, जिसमें भगवान् का विशिष्ट प्रकाश है उसे विभूति कहते हैं। जैसे कि अर्जुन भगवान् की विभूति था। श्रीकृष्ण स्वयं को भी विभूति बताते हैं। विभूति और अवतार में अन्तर यह है कि अवतार को स्वयं के विषय में पता रहता है कि वह अवतार है परन्तु विभूति को स्वयं के बारे में पता नहीं रहता।
प्रश्न : अवतार के प्रमुख क्रिया-कलाप तथा उद्देश्य क्या होते हैं?
उत्तर : गीता के श्लोकों से तो इसका अर्थ यह लगता है कि -
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जब-जब धर्म क्षीण हो जाता है और अधर्म ऊपर को उठ जाता है (बढ़ जाता है) तब मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।।
साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में जन्म लेता हूँ।
श्रीअरविन्द का कहना है कि अवतार के जन्म ग्रहण के लिये ये कोई भी पर्याप्त उद्देश्य नहीं हैं। और यदि हम गीता की शिक्षा को व्यापक रूप में लें तो इसका अधिक गहरा अर्थ निकल कर आता है। किसी भी धर्म की संस्थापना के लिए, साधु-पुरुषों की रक्षा करने के लिए या दुष्टों के विनाश के लिए स्वयं भगवान् को आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये कार्य तो वे अपनी किसी विभूति के द्वारा या परिस्थितियों के सहारे भी साधित करा सकते हैं। इसलिये इनमें से कोई भी प्रयोजन अवतार के आने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इस तरीके से तो यदि पहले किसी भी व्यक्ति ने कोई महान् काम किया हो तो उसे अवतार बता दिया जाएगा। गीता में इस तरीके की कोई बात नहीं है। गीता के अन्दर तो इसका बहुत गहरा और दिव्य रहस्य है।
इसमें गीता कहती है कि भगवान् की अभिव्यक्ति जो अवतार के द्वारा होती है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि भगवान् स्वयं धरती पर अवतार लेकर साधारण मानवीय मन, प्राण, शरीर को धारण करते हैं। यह तो भगवान् का शाश्वत अवतार है। दूसरे पहलू में जब मनुष्य स्वयं विकसित होकर बाहरी प्रकृति की पाश में न रहकर आत्मा में नवजन्म ग्रहण करता है, उसे द्विज कहते हैं। और इससे वह भगवान् की चेतना के निकट पहुँचता है। श्रीअरविन्द का कहना है कि गीता में मनुष्य का जो दूसरा जन्म बताया गया है, जो कि भगवान् की ओर आरोहण है और जो सारी सृष्टि का उद्देश्य है, उसमें सहायता करने के लिए ही अवतार आते हैं क्योंकि भगवान् की ओर आरोहण का उद्देश्य अन्य किसी तरीके से इतनी आसानी से पूरा नहीं हो सकता। उस आरोहण के लिए मनुष्य को जीवंत उदाहरण की, भगवान् के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तभी वह इसे कर पाता है। और आवश्यकता की पूर्ति के लिए अवतार की अभिव्यक्ति होती है। श्रीमाताजी ने भी अवतारों के उद्देश्य के विषय में बताया है। उसकी चर्चा बाद में आएगी।
केवल इन दो श्लोकों से यह बात स्पष्टतया सामने नहीं आती इसलिए श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि केवल सतही तौर पर पढ़ने से नहीं अपितु गहराई से पढ़ने पर ही यह बात समझ में आ सकती है।
अवतार तत्त्व का रहस्य बड़ा ही गहरा है। जब स्वयं भगवान् ही कहते हैं कि 'जन्म कर्म च मे दिव्यं', मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं और जो इस को जान लेता है वह फिर दुबारा जन्म नहीं लेता, तो अवश्य ही यह एक ऐसा विलक्षण रहस्य होना चाहिये जिसे जानकर व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता, क्योंकि केवल यह जान लेने भर से कि भगवान् श्रीकृष्ण, श्रीराम आदि अवतार हैं, किसी का कल्याण नहीं हो जाता और न ही व्यक्ति को मुक्ति ही मिल सकती है। इसलिये ये सारी बातें रहस्यमयी हैं। इस रहस्य को श्रीअरविन्द धीरे-धीरे खोलने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रश्न : क्या इस बात को सावित्री की इन पंक्तियों के साथ जोड़ा जा सकता है कि :
'हम भगवान् के पुत्र हैं और अवश्य ही उनके सदृश होना होगाः उनके मानवीय अंश हम, हमें दिव्य बनना है।' (Savitri, p.67)
उत्तर : इस क्रमविकास को तो श्रीअरविन्द मान ही रहे हैं। परंतु सावित्री में अवतार के अवतरण की बात नहीं है। वह तो क्रमविकास की बात है। जब भगवान् स्वयं चेतना के अंतर्वलयन (involution) के द्वारा ये सब जड़पदार्थ और जीव जगत् बन गए हैं तो वे यहीं नहीं रुकेंगे, चेतना के विकास के द्वारा वे पुनः अपने निज-स्वरूप की ओर जाएँगे। परंतु अवतार के आविर्भाव की बात विशेष है। 'वह' जो एक असीम चेतना है वह मनुष्य शरीर धारण कर के प्रकट हो जाती है। रामायण, भागवत् आदि हमारे सभी सद्ग्रंथों का यही कहना है कि अवतार का विद्यमान होना तो स्वयं परम् पुरुष परमेश्वर का उपस्थित होना है। यह कोई आंशिक या धुँधली-सी उपस्थिति नहीं है। यह तो परमोच्च प्रभु की पूर्ण विद्यमानता है। तुलसीदास जी भी भगवान् श्रीराम को चरम-परम बताते हैं। अवतार भगवान् की भौतिक उपस्थिति, उनकी सशरीर विद्यमानता है। श्रीअरविन्द ने भी इसी बात की संपुष्टि की है। वे श्रीमाताजी को परम् दिव्य जननी जगदम्बा बताते हैं। उनके अनुसार, "वे 'एक' जिन्हें हम श्रीमाताजी के रूप में पूजते हैं, भागवती चित्-शक्ति हैं जो अखिल अस्तित्व का शासन करती हैं, जो एक होते हुए भी इतनी बहुमुखी हैं कि उनकी गति का अनुसरण कर पाना तीव्रतम मन और मुक्ततम तथा अत्यंत विशाल बुद्धि तक के लिए भी असंभव है। श्रीमाताजी परमोच्च की चेतना और शक्ति हैं और जो कुछ वे सृष्ट करती हैं स्वयं उससे बहुत ऊपर हैं।" (CWSA 32, p.2)
यही भागवत् का वचन है कि परात्पर, पुरुषोत्तम, परमात्मा, परंब्रह्म, परमेश्वर ने स्वयं मानव शरीर धारण किया है। यह तो बड़ी ही विलक्षण बात है जो बुद्धि के लिए समझ पाना बहुत ही भारी है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हमारे पुराणों में भी इस तरीके के संकेत हैं। यहाँ भी श्रीअरविन्द इस बात का लगभग समर्थन करते प्रतीत होते हैं। और इस अवतार तत्त्व से क्रमविकास में तो सहायता मिलती ही है। यदि श्रीमाताजी का आविर्भाव न हुआ होता तो पृथ्वी पर उनके आगमन से जो इतना महत् कार्य संसिद्ध हुआ और जो अब भी हो रहा है तथा आगे भी होगा, वह न हो पाता। उनके आगमन से महान् अभ्युदय हुआ, साधना का अत्यंत विशाल मार्ग उद्घाटित हुआ। वे कोई दुष्टों का संहार करने थोड़े ही आईं थीं। इस तरीके की तो कोई बात थी ही नहीं। इसी प्रकार श्रीरामकृष्ण, श्रीचैतन्य महाप्रभु आदि सभी ने क्रमविकास को आगे बढ़ाने में महत् योगदान किया व अब भी अभूतपूर्व रूप में कर रहे हैं।
अवतार मानव-प्रकृति में भागवत् प्रकृति के आविर्भाव के रूप में आता है, अपने ईसा, कृष्ण और बुद्ध तत्त्व को प्रकट करने के लिए, जिससे कि मानव-प्रकृति अपने सिद्धांत, विचार, अनुभव, कर्म और सत्ता को ईसा, कृष्ण और बुद्ध के भाव में ढालकर स्वयं को भागवत् प्रकृति में रूपांतरित कर4. अवतार-तत्त्व की संभावना सके।... हम कह सकते हैं कि मानव के रूप में भगवान् के प्राकट्य की सम्भावना को दृष्टांतरूप से सामने रखने के लिए अवतार होता है, ताकि मनुष्य देख सके कि यह क्या तत्त्व है और उस तत्त्व के स्वरूप में विकसित होने का साहस कर सके। और यह (अवतार ग्रहण) इसलिए भी होता है कि इसके बाद इसके आविर्भाव या प्राकट्य के प्रभाव को पार्थिव-प्रकृति में स्पंदित रखा जा सके और पार्थिव-प्रकृति के ऊर्ध्वमुख परिश्रम का उस आविर्भाव के सारतत्त्व द्वारा संचालन किया जा सके। यह मानव की जिज्ञासु आत्मा को दिव्य मानवता का आध्यात्मिक साँचा प्रदान करने के लिए होता है जिसमें कि वह अपने-आप को ढाल सके। यह जन्म एक धर्म प्रदान करने के लिए - केवल कोई संप्रदाय या मतविशेषमात्र नहीं, अपितु आंतर और बाह्य जीवनयापन की प्रणाली प्रदान करने के लिए - आत्म-संस्कारक मार्ग, नियम और विधान प्रदान करने के लिए होता है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्यता की ओर बढ़ सके। चूंकि यह विकास, यह आरोहण कोई अलग-थलग और वैयक्तिक विषय या क्रिया नहीं है, अपितु भगवान् की समस्त जगत्-क्रियाओं की भाँति ही एक सामूहिक क्रिया-व्यापार है, मानवजाति के लिये किया गया कर्म है, अतः अवतार मानव-यात्रा में सहायता करने के लिए, महान् संकट-काल के समय इसे थामे रखने के लिए, अधोगामी शक्तियाँ जब बहुत अधिक बढ़ जायें तो उन्हें छिन्न-भिन्न करने के लिए, मनुष्य के अन्दर जो भगवन्मुखी महान् धर्म है उसकी स्थापना या रक्षा करने के लिए, भगवान् के साम्राज्य की (फिर चाहे वह कितना ही सुदूर क्यों न हो) प्रतिष्ठा के लिए, प्रकाश और पूर्णता के साधकों (साधूनां) को विजय दिलाने और जो अशुभ और अंधकार को बनाये रखने के लिए संघर्ष करते हैं उनका विनाश करने के लिए होता है। अवतार के ये हेतु सर्वमान्य हैं और प्रायः उसके कर्म को देख कर ही जनसमुदाय उन्हें विशिष्ट पुरुष के रूप में जानता और पूजने को तैयार होता है। केवल आध्यात्मिक जन ही हैं जो यह देख पाते हैं कि एक मानव जीवन के प्रतीक के रूप में यह बाह्य अवतारत्व उस शाश्वत आंतरिक देवत्व का चिह्न है जो उनकी (मनुष्यों की) अपनी मानसिकता और भौतिकता के क्षेत्र में स्वयं को अभिव्यक्त करता है जिससे कि वे उसके साथ अधिकाधिक एकत्वमय हो सकें और उसके द्वारा अधिकृत हो जाएँ। बाह्य मानवरूप में ईसा, बुद्ध या कृष्ण का जो दिव्य प्राकट्य होता है उसके अंदर आंतरिक सत्य के रूप में निगूढ़ सनातन अवतार की वही अभिव्यक्ति होती है, जो हमारी अपनी आंतरिक मानवीयता में भी होती है। जो कुछ अवतारों के द्वारा इस पृथ्वी के बाह्य मानव-जीवन में किया गया है वह समस्त मानव-प्राणियों के अन्दर दोहराया जा सकता है।
इसमें अवतार के जन्म ग्रहण के सारे हेतु बता दिए गए हैं। जैसे कि, साधुओं की रक्षा, अशुभ आदि बाधाओं को दूर करना, दुष्टों का विनाश करना और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना जिससे मनुष्य प्रेरित होकर उस रास्ते पर चल सकें। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब धरती पर अवतार का आर्विभाव होता है तब उनकी उपस्थिति धरती के सूक्ष्म वातावरण पर भी इस तरह अपनी छाप छोड़ती है, मनुष्यों के हृदय और बुद्धि में इतनी जगह बना लेती है कि उसको उपयोग में लेकर मनुष्य के जीवन में सतत् रूप से दिव्य, आध्यात्मिक प्रभाव प्रवेश कर सकता है। श्रीराम, श्रीकृष्ण, ईसा और बुद्ध का प्रभाव आज भी पृथ्वी के सूक्ष्म वातावरण में विद्यमान है। यदि उनका प्रभाव केवल उनके आविर्भाव के समय ही होता और बाद में न रहता तब तो अवतार का आना निष्फल ही होता क्योंकि जब वे आविर्भूत हों तब उस समय विशेष के लिये तो पृथ्वी का वातावरण प्रभावित होगा परंतु उनके तिरोहित होने के बाद वह यथावत् ही हो जाएगा। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं रहने पर भी वे स्वयं सूक्ष्म भौतिक जगत् में विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के लिए आज के समय में भी श्रीरामजी, श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसा का बड़ा भारी प्रभाव है, जिनसे मनुष्यों को सतत् रूप से प्रेरणा मिलती रहती है और वे भगवान् की ओर आरोहण करते हैं।
श्रीमाताजी अवतार के बारे में जो बताती हैं वह बात और भी विलक्षण है जिसका हमारे पुराणों में भी संकेत मिलता है, कि जब भगवान् का अवतरण हुआ तो उनके संपर्क मात्र में आने से गोपियों का तथा अन्यान्य लोगों का परम् कल्याण हो गया। इसलिए भगवान् के साथ संपर्क होना ही बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने लिये तो यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। श्रीमाताजी के संपर्क मात्र में आने से लोगों का सारा जीवन ही बदल गया, जबकि जिसे लोग साधना या योग कहते हैं ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। ऐसे लोग जो कभी भगवान् की ओर चल ही नहीं सकते थे, जिनके जीवन में साधना से कोई सरोकार ही नहीं था, उन लोगों का भी केवल श्रीमाताजी के संपर्क में आने से और उनकी सेवा करने से सारा जीवन ही बदल गया। इसलिए उनके संपर्क में आने और उनसे संबंध रखने का बड़ा भारी महत्त्व है। आज भी श्रीअरविन्द आश्रम का सारा काम श्रीमाताजी के सूक्ष्म संपर्क और उनके प्रति भक्ति से ही चल रहा है अन्यथा आश्रम की इतनी विशाल व्यवस्था सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती थी। इसलिए यह तो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अवतार की क्या महत्ता है। उनकी उपस्थिति सदा बनी रहती है, संचालन करती है और जहाँ जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की पुकार होती है, उसमें जिस प्रकार का खुलाव होता है, जैसा उसका गठन होता है, उसी प्रकार उसकी सहायता करती है। जितने भी प्रमुख अवतार हुए हैं उनकी सूक्ष्म उपस्थिति मात्र से लाखों-करोड़ों व्यक्ति परमात्मा के रास्ते पर लगे हुए हैं। यह एक प्रकार का राजमार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति भगवान् तक पहुँचता है।
सबसे विलक्षण बात यह है जो हमारे पुराण बार-बार में समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान् के श्रीविग्रह से किसी भी तरह से संपर्क में आ जाना। यदि उनकी उपस्थिति सूक्ष्म भौतिक जगत् में है और वे सशरीर उपस्थित नहीं हैं, तो भी उनकी कथाओं, लीलाओं, चर्चाओं आदि के माध्यम से उनके संपर्क में आ जाना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार तीर्थस्थलों का भी बहुत भारी महत्त्व है क्योंकि वे बार-बार हमें भगवान् के श्रीविग्रह की, उनकी लीलाओं की याद दिलाते हैं कि भगवान् ने अमुक स्थान पर रास किया था, अमुक लीला की थी। अमुक स्थान पर भगवान् शिव प्रकट हुए, अमुक स्थान पर सती जी ने अपने शरीर को भस्म किया था। इसी प्रकार सभी शक्तिपीठ हमें देवी की लीलाओं-कथाओं का स्मरण कराते हैं। इससे उनके साथ कुछ-न-कुछ संपर्क अवश्य साधित हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में तीर्थस्थलों को, सभी अनुष्ठानों आदि को इतना अधिक महत्त्व दिया जाता था और पूरा जीवन ही इन अनुष्ठानों आदि से रंग दिया जाता था।
हमारे ऋषियों को यह गहरा बोध था कि यदि व्यक्ति को भगवान् के सशरीर विग्रह के दर्शन न भी हो रहे हों तो कम-से-कम उनकी लीला-कथा सुन कर भावात्मक रूप से उनके साथ जुड़ सकता है। हम उनकी वृंदावन की लीलाएँ सुन सकते हैं, माखन चोरी की कथाएँ, भिन्न-भिन्त्र दुष्टों के संहार की लीलाएँ, गोवर्धन पर्वत को उठाने की कथाएँ सुनकर गद्गद् हो सकते हैं। इसीलिए पूरे भारत में सप्ताह श्रवण आदि अनेकों प्रकार के अनुष्ठान आज भी प्रचलित हैं जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कर के भगवान् के संपर्क में आते हैं।
जप, तप और ध्यान आदि अभ्यासों को करने से तो व्यक्ति अहं से भर सकता है परन्तु भगवान् की दिव्य कथाओं को सुनने में तो अहं को अपनी तुष्टि का अवसर ही नहीं मिलता। उनकी लीलाएँ सुनने में तो केवल आनन्द ही आनन्द है। इसमें अहं के लिए कहाँ स्थान है, इसमें तो हमारा हृदय भगवान् की ओर खिंचता है और केवल उन्हीं की स्मृति बनी रहती है। तो इस सब के पीछे यह परम् रहस्य है।
इन सभी चीजों के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से भगवान् के श्रीविग्रह के साथ जुड़ाव। वह जिस किसी तरीके से हो, पर महत्त्वपूर्ण चीज है उनके संपर्क में आ जाना। हमारे तंत्रों ने तो भगवान् का मूर्तिकरण कर दिया। उनकी भावना कर के व्यक्ति उनकी सेवा कर सकता है, भोग अर्पित कर सकता है। यह तो उनसे संपर्क साधने का अत्यंत शक्तिशाली तरीका है। श्रीअरविन्द आश्रम में भी यही बात थी कि किसी भी तरीके से श्रीमाताजी के साथ संपर्क में आ जाना। उन्हीं के लिए काम करना, उन्हीं के निमित्त अपनी सारी चेष्टाएँ करना। वहाँ साधना का सारा आधार ही यही था और आज भी यही है। आश्रम में कोई व्यक्ति खेती में व्यस्त है, कोई खाना पकाने में व्यस्त है, कोई पुस्तकें छापने में व्यस्त है तो अन्य कोई किसी दूसरे कार्य में व्यस्त है। कुछ को तो किसी प्रकार के ध्यान या अन्य किसी प्रकार की किसी साधना के लिए कोई समय ही नहीं है।
अवतार-तत्त्व का यही गहरा औचित्य है कि जिस भी तरीके से हो भगवान् के साथ भौतिक संपर्क में आ जाना। हमारा भौतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से भगवान् के साथ संपर्क बड़ी महत्त्वपूर्ण चीज है। जब दिलीप कुमार रॉय ने श्रीअरविन्द को लिखा कि कृष्ण-चेतना तो अवश्य ही बड़ी महान् चीज है पर कृष्ण का वास्तव में क्या अर्थ है। तो श्रीअरविन्द ने उत्तर दिया कि बिना कृष्ण के कृष्ण की चेतना कैसे हो सकती है। भगवान् श्रीकृष्ण तो स्वयं सूर्य के समान हैं और उनके सामने ब्रह्म, सच्चिदानंद आदि तो ऐसे हैं जैसे कि सूर्य का प्रकाश। बिना सूर्य के उसका प्रकाश कहाँ से आएगा। जो चीज वास्तविक है और जिससे सारी चीज प्रस्फुटित होती है उसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। इसी तत्त्व को सर्वगुह्यतम् बताते हुए भगवान् गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा। इसी से भगवान् की व्यक्तिगत उपस्थिति का, उनके साथ संपर्क का महत्त्व पता चल जाता है।
-------------
... प्रत्येक जीव अपने नव जन्म में एक नवीन मन, प्राण और शरीर तैयार करता है - अन्यथा जॉन स्मिथ सदा जॉन स्मिथ ही बना रहेगा और उसे कभी पीयूषकांति घोष बनने का सुयोग नहीं प्राप्त होगा। निःसन्देह, भीतर पुराने व्यक्तित्व बने रहते हैं जो नये जीवन में अपना योगदान करते हैं- परंतु मैं नवीन प्रत्यक्ष व्यक्तित्व को, मन, प्राण और शरीरमय बाह्य मनुष्य को बात कर रहा हूँ। यह चैत्य पुरुष ही है जो एक जन्म से दूसरे जन्म की कड़ी को बनाये रखता है और उस एक व्यक्ति की समस्त अभिव्यक्तियों को संसिद्ध करता है। इसलिये यह अपेक्षित ही है कि अवतार प्रत्येक बार एक नया व्यक्तित्व ग्रहण कर सकता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो नये समय, कार्य और परिस्थितियों के अनुकूल हो। हालाँकि वस्तुओं के मेरे अपने दृष्टिकोण के अनुसार इस नये व्यक्तित्व के पीछे अवतार के जन्मों की एक श्रृंखला होती है, ऐसे जन्म जिनमें मध्यवर्ती विकासक्रम का अनुसरण किया गया होता है और युग-युग में सहायता दी गई होती है।
प्रश्न: कथा आदि में तो हम देखते हैं कि आजकल केवल पैसे का ही लेनदेन हो गया है, तो इसमें क्या कोई सच्चा संपर्क हो सकता है?
उत्तरः अवश्य ही इतने सारे लोगों के बीच कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें उससे कुछ-न-कुछ भगवान् से संपर्क साधने में सहायता मिलती है। साथ ही, इस विषय में हम बाहरी रूप से तय नहीं कर सकते। हो सकता है कि सतही रूप से तो व्यक्ति समझ न रहा हो, परंतु चैत्य को उसमें रस आ रहा हो। इसलिए ये बड़ी ही जटिल चीजें हैं जिनके विषय में कोई सीधा सरल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब जैसे गंगा स्नान का अपना महत्त्व है। भले हम विश्वास करें या न करें पर जब भी हम उसमें स्नान करते हैं तो अवश्य ही हमारे पाप क्षय होते हैं और चेतना उद्बुद्ध और विकसित होती है। यह तो उन लोगों द्वारा प्रमाणित किया गया तथ्य है जो इसमें पहले तो विश्वास नहीं करते थे परंतु जब उन्होंने स्वयं इसे परखा तब जाकर इसमें विश्वास करना आरंभ किया। ये सभी सजीव उपस्थितियाँ हैं जिनसे व्यक्ति संपर्क में आ सकता है और यदि वह थोड़ा-बहुत भी आंतरिक रूप से विकसित हो, तब तो उसे उनका जीवंत अनुभव भी हो सकता है।
अवतार लेने का यही उद्देश्य होता है, परंतु इसकी प्रक्रिया क्या है? सर्वप्रथम, अवतार के विषय में एक तर्कसंगत या संकीर्ण विचार है जो इसमें ऐसे नैतिक, बौद्धिक और क्रियात्मक दिव्यतर गुणों की केवल एक असाधारण अभिव्यक्तिमात्र देखता है, जो गुण औसत मानवजाति का अतिक्रम कर जाते हैं। इस विचार में कुछ सत्य है। अवतार साथ-ही-साथ विभूति भी तो हैं।... गीता में भगवान् कहते हैं, "वृष्णियों में मैं वासुदेव (श्रीकृष्ण) हूँ, पांडवों में धनञ्जय (अर्जुन) हूँ, मुनियों में व्यास और द्रष्टा कवियों में उशना कवि हूँ", प्रत्येक कोटि में सर्वश्रेष्ठ, प्रत्येक वर्ग में महत्तम, अर्थात् विभूति उन गुणों और कर्मों की अत्यंत शक्तिशाली प्रतिनिधि होती है जिनसे वह वर्गविशेष स्वयं की विशिष्ट आत्मशक्ति को प्रकट करता है। सत्ता की शक्तियों का यह उत्कर्ष भागवत् प्राकट्य के क्रम में अत्यंत आवश्यक चरण है। प्रत्येक महापुरुष जो हमारे औसत स्तर से ऊपर उठ जाता है, वह इसी कारण हमारी सामान्य मानवीयता को ऊपर उठा देता है; वह हमारी दिव्य संभावनाओं का एक जीवंत दृढ़ आश्वासन, परमेश्वर का एक वचन, दिव्य ज्योति की एक प्रभा तथा दिव्य शक्ति का एक उच्छ्वास होता है।
व्यक्ति का जन्म कैसे होता है? अवतार कैसे जन्म ग्रहण करता है? अवतार का अर्थ है वह जिसमें विशेष प्रतिभा हो, विशेष गुण हों, विशेष चीजें हों। जो विशेष गुण विभूति में होते हैं वे अवतार में और भी अधिक विशेष रूप से होते हैं, क्योंकि अवतार साथ-ही-साथ विभूति भी तो है। यह अवतार के विषय में एक मूलभूत बात है। गीता के दृष्टिकोण पर हम बाद में आयेंगे। यह एक बात हो गयी। एक दूसरी बात यहाँ यह आई है कि व्यक्ति अलग-अलग जन्म कैसे ग्रहण करता है? और अवतार तथा व्यक्ति के जन्म के बीच क्या अंतर है? जहाँ तक व्यक्ति के जन्म की बात है, श्रीअरविन्द कहते हैं कि कोई ऐसी गहरी चीज, हमारी चैत्य सत्ता, होती है जो विभिन्न जन्मों की श्रृंखला के अंदर विकसित होती है। उदाहरण के लिये व्यक्ति एक जन्म में कुछ प्राप्त करता है, कुछ गहरे अनुभव अर्जित करता है, इन सब में जो सच्ची चीज होती है, वह कुछ हद तक बची रह जाती है, शेष बाहरी आवरण पंचभूतों में विलीन हो जाता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो साधारणः पहले भौतिक देह छूट जाती है, फिर प्राणिक देह, फिर मानसिक देह और तब हमारा चैत्य पुरुष चैत्य जगत् में लौट जाता है। जन्म के दौरान जो चैत्य क्षण हमने जीये, जिनमें कि चैत्य भाग को अनुभव प्राप्त हुए, वे सुरक्षित रह जाते हैं। जब हम नया जन्म लेते हैं, तो उस अमुक जन्म में चैत्य की अभिव्यक्ति किस प्रकार की होनी है उसके अनुसार हमें नया मन-प्राण-शरीर प्राप्त होता है। इसलिये साधारणतः हमें पुरानी कोई स्मृति नहीं रहती। और चूंकि हम अधिकांशतः अपने मन, प्राण और शरीर की चेतना में ही निवास करते हैं इसलिये उनके विलोप के साथ ही सब कुछ लुप्त हो जाता है। परंतु जो चैत्य क्षण हमने उस पिछले जन्म में आरक्षित कर लिये थे और जो उपयोगी थे वे वर्तमान व्यक्तित्व में भी मौजूद रहते हैं और काम कर रहे होते हैं। हम यदि उस भाग में जा सकें तो हमें वे क्षण और उनके साथ जुड़ी चीजें कुछ याद आ सकती हैं। ठीक-ठीक घटनाओं की तो स्मृति नहीं परन्तु व्यक्ति को महसूस हो जाता है कि वे ऐसे थे, ये ऐसा था। ऐसी कुछ चीजें याद आ सकती हैं। बिल्कुल सभी घटनाएँ भी याद आ सकती हैं परंतु वह एक अलग चीज है। वह स्मृति तो पृथ्वी की गुह्य-स्मृति में प्रवेश करने पर ही पुनः प्राप्त हो सकती है। परंतु इसकी चर्चा विषयांतर होगी।
हमारे पहले के जितने भी जन्म हैं, उनके व्यक्तित्वों में से जो चैत्य-तत्त्व आरक्षित रह गये हैं वे सभी वर्तमान में क्रियारत हैं। इसीलिए अपने वर्तमान जन्म में हम कभी तो क्या कर बैठते हैं, और कभी कुछ और; कभी हमें कोई अप्रत्याशित अनुभव प्राप्त हो जाता है, कभी कोई विचित्र चीज आ उपस्थित होती है। इस प्रकार हम केवल इस जन्म से ही चालित नहीं हैं क्योंकि वे सारे तत्त्व पृष्ठभूमि में काम कर रहे होते हैं और व्यक्ति तो मुखौटा मात्र ही है। साधारण रूप से यह तो जीवनों की श्रृंखला से होते हुए एक व्यक्ति के चैत्य पुरुष के विकास की बात हो गयी।
अब अवतार के बारे में श्रीअरविन्द का दृष्टिकोण है कि, "...यह अपेक्षित ही है कि अवतार प्रत्येक बार एक नया व्यक्तित्व ग्रहण कर सकता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो नये समय, कार्य और परिस्थितियों के अनुकूल हो।" अवतार एक नया व्यक्तित्व लेगा, उसका पहले का ही व्यक्तित्व नहीं होगा, “...हाँलाकि वस्तुओं के मेरे अपने दृष्टिकोण के अनुसार इस नये व्यक्तित्व के पीछे अवतार के जन्मों की एक श्रृंखला होती है, ऐसे जन्म जिनमें मध्यवर्ती विकासक्रम का अनुसरण किया गया होता है और युग-युग में सहायता दी गई होती है।" जैसा कि श्रीमाताजी एक स्थान पर कुछ यूँ कहती हैं, 'मैं और श्रीअरविन्द सदा ही मौजूद रहे हैं। हर युग में हमने सहायता दी है।' परन्तु वे सदा ही अवतार के रूप में मौजूद नहीं थे। जन्मों की एक श्रृंखला होती है, परन्तु व्यक्ति का सभी जन्मों में अवतार होना आवश्यक नहीं है। जहाँ-जहाँ भी उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता थी वहीं श्रीमाँ व श्रीअरविन्द ने सहायता प्रदान की थी, हालाँकि अवतार के रूप में नहीं। अवतार में तो उन सभी जन्मों की पराकाष्ठा हो जाती है। उसके पूर्व के जो जन्म होते हैं उनमें अवतार के गुण नहीं होते जैसे कि कहा जाता है कि श्रीमाताजी पूर्व जन्म में कैथरीन द ग्रेट थीं, श्रीअरविन्द पूर्वजन्म में अगस्तस सीज़ थे। उन जन्मों में वे अवतार रूप में नहीं थे। इसलिए पूर्वजन्मों की श्रृंखला में समय-समय पर अपना योगदान देने और क्रमविकास में सहायता प्रदान करने पर भी आवश्यक नहीं है कि उन जन्मों में उनमें अवतार तत्त्व हो। इसलिए अवतार नया व्यक्तित्व ग्रहण करते हैं, पहले के व्यक्तित्वों को दोहराते नहीं। हमारे हिन्दु-धर्म में यह मान्यता है कि श्रीराम ही श्रीकृष्ण के रूप में आये थे। परन्तु हम देख सकते हैं कि उनके गुणों में एक दूसरे से कितनी भिन्नता थी, बाहरी व्यक्तित्व सर्वथा भिन्न थे।
वैसे ही भगवान् बुद्ध से पहले अनेक बोधिसत्त्व हुए थे। इसमें विचारने योग्य बात यह नहीं है कि भगवान् बुद्ध से पहले बोधिसत्त्व हुए थे या नहीं, अपितु यह है कि अवतार की जो कथाएँ हैं, जो लीलाएँ हैं, उनके पीछे एक बड़ा भारी औचित्य है, उनका महत्त्व है। जिन लोगों को इन चीजों का थोड़ा-सा भी आभास है वे एक ऐसे प्रतीक के रूप में ऐसी चीज प्रकट करना चाहते हैं, जो सत्य है। चाहे वे चीजें भौतिक जगत् में उस तरह से घटित हुई हों या नहीं, उसका महत्त्व नहीं है क्योंकि अवतार अपनी भौतिक अभिव्यक्ति से सीमित नहीं है। उसकी क्रिया तो बहुत विशाल है। अन्यथा तो उसका महत्त्व केवल उसके जीवन काल तक ही सीमित रहता और उससे अधिक उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। एक बार भौतिक जगत् से प्रयाण के बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता। तो अवतार की जो बातें हैं, उनका जो सत्य है, उन्हें ऐसे रूपकों में, कथाओं में, प्रतीकों में इस तरह प्रकट किया जाता है कि वह मनुष्य की आत्मा में प्रवेश कर जाता है और वहाँ अपना प्रभाव फैलाता है। मूलतः हमें यह समझना होगा कि अवतार भगवान् का सव्यक्तिक या साकार पहलू है। योगी श्री कृष्णप्रेम पुस्तक में इस विषय पर श्रीअरविन्द के पत्र हैं। अवतार में जो महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, वह उनकी शिक्षा, उनके क्रियाकलाप आदि नहीं है, अपितु वह है उनके अंदर अभिव्यक्त होता परमात्मा का व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व की सुंदरता, उस व्यक्तित्व के विभिन्न क्रियाकलाप जिन्हें प्रतीकों में अभिव्यक्त तो किया जा सकता है परन्तु उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वे अवर्णनीय चीजें हैं। वे प्रतीकों के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त हो जाती हैं। और ये प्रतीक भी इस तरह बनाये जाते हैं जिससे कि मनुष्य अपने हृदय, प्राण, मन में उन्हें पकड़ सके। अतः अवतार की महत्ता उनकी शिक्षा अथवा उन्होंने यदि कोई साधना की है तो उसमें नहीं है, उनकी महत्ता तो उनके अंदर के उस परमात्म तत्त्व में है जो उनमें अभिव्यक्त हो रहा है और जो इस भौतिक और सूक्ष्म भौतिक जगत् तक पर अपनी इतनी भारी अमिट छाप छोड़ता है। उनकी शिक्षा तो आखिर में उसी परमात्म तत्त्व की ओर चलने के लिए और उसे अभिव्यक्त करने के लिए होती है। सारी आध्यात्मिक सिद्धि, साधना आदि उनकी ओर चलने वाली गतियाँ मात्र हैं जो वास्तव में तो उन्हें कभी प्राप्त नहीं करतीं, जबकि स्वयं अवतार में तो परमात्मा का व्यक्तित्व होता है और यही विलक्षण चीज है। इसकी महत्ता की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। दिलीप कुमार रॉय को लिखे अपने पत्र में श्रीअरविन्द लिखते हैं कि, "मुझे लगता है कि आधुनिक लोग जो अवतार की जीवन-चरितसंबंधी और ऐतिहासिक बातों पर अर्थात् उनके जीवन के बाहरी तथ्यों पर, उनके बाहरी जीवन की घटनाओं पर जोर देते हैं उनमें एक मौलिक भूल है। महत्त्वपूर्ण चीज है वह आध्यात्मिक सत्य, शक्ति और प्रभाव जो उनके साथ आते हैं अथवा जिन्हें वे अपने कर्म और जीवन के द्वारा नीचे उतार लाते हैं।... उसका आंतरिक जीवन ही उसके बाहरी जीवन को कुछ महत्त्व प्रदान करता है। उसका आंतरिक जीवन ही उसके बाहरी जीवन को शक्ति देता है जो उसमें हो सकती है और आध्यात्मिक मनुष्य का आंतरिक जीवन एक विशाल और पूर्ण वस्तु होता है और, कम-से-कम महान् पुरुषों में, अर्थपूर्ण चीजों से इतना अधिक परिपूर्ण, इतने घने रूप में भरा होता है कि कोई भी जीवनी-लेखक या इतिहास लेखक उन सब को पकड़ पाने और कह पाने की कभी आशा भी नहीं कर सकता। उसके बाहरी जीवन में जो कुछ महत्त्वपूर्ण होता है वह इसलिये होता है कि वह उस चीज का प्रतीक होता है जिसे उसने स्वयं अपने भीतर उपलब्ध किया है और हम और भी आगे बढ़कर कह सकते हैं कि उसका आंतरिक जीवन भी उसके पीछे विद्यमान भगवत्तत्त्व की क्रिया की एक अभिव्यक्ति, एक जीवंत प्रतिमूर्ति के रूप में ही महत्त्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि हमें यह खोज करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या श्रीकृष्ण-संबंधी कहानियाँ पृथ्वी पर किये गये उनके कार्यों का, चाहे जितना भी अपूर्ण, वर्णन है अथवा जो कुछ श्रीकृष्ण मनुष्यों के लिये थे या हैं उसका, तथा श्रीकृष्ण के रूप में अभिव्यक्त भगवान् का प्रतीकात्मक चित्रण है।... ईसा और बुद्ध के विषय में जो कुछ बाहरी तथ्य वर्णित हैं वे अन्य बहुत से लोगों के जीवन में घटित तथ्यों से बहुत अधिक नहीं हैं - फिर भला वह कौन सी चीज है जो बुद्ध या ईसा को आध्यात्मिक जगत् में बहुत ऊँचा स्थान प्रदान करती है? उन्हें जो यह स्थान मिला उसका कारण यह था कि उनके द्वारा कुछ ऐसी चीज अभिव्यक्त हुई जो किसी भी बाहरी घटना या किसी भी शिक्षा से बहुत अधिक थी।" (योगी श्रीकृष्णप्रेम, पृष्ठ १९१-९२)
इसलिए अवतार का व्यक्तित्व ऐसी महत्त्वपूर्ण चीजों से लबालब होता है जिन्हें कदाचित् ही कोई देख सकता हो परंतु फिर भी वे इस पार्थिव प्रकृति में अभिव्यक्त हो जाती हैं। और वे इस तरह से अभिव्यक्त हो जाती हैं कि कथा, कहानियों, रूपकों आदि के माध्यम से जैसे ही हमें उनका संकेत प्राप्त होता है वैसे ही उनसे एक संपर्क साधित हो जाता है। और जरा से सम्पर्क का भी बड़ा गहरा प्रभाव होता है। यदि हमारा उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क साधित हो जाएगा, दिल से दिल मिल जाएगा, तब तो उसके प्रभाव का तो कहना ही क्या है।
सोचिये कि हमारे पास यदि श्रीमाँ व श्रीअरविन्द की केवल शिक्षा ही होती, या कोई हमें उनकी शिक्षा बता देता या सुना देता परंतु स्वयं श्रीमाँ की जीवंत उपस्थिति हमारे पास न होती तब तो सब कुछ वीरान ही होता। तब फिर हमारे लिए उनकी सारी शिक्षा आदि का विशेष कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। उस व्यक्तित्व के बिना केवल उस शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं। इस सब का महत्त्व तो केवल इस बात से है कि स्वयं जगदंबा ने शरीर धारण किया था, और यह एक ऐसी विलक्षण बात है जो हमारी सोच-समझ से सर्वथा परे है। यही मुख्य चीज है, यही बात इस अवतार तत्त्व को धरती के लिये परम महत्त्व की बना देती है। अवतार तत्त्व के साथ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनकी कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, किसी भी आध्यात्मिकता में, कैसे भी बड़े - से - बड़े अनुभव में उनको पकड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि हमारी आध्यात्मिकता आदि से तो परमोच्च सत्ता कहीं परे है। वह तो बहुत ऊँचा स्तर है। और जब अवतार उस परम के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कर रहा हो तब फिर उसके संबंध में तो कुछ कहा ही क्या जा सकता है। भले ही भगवान् वराह के रूप में ही क्यों न हों तो भी उनके सामने अतिमानसिक सत्ता की भी क्या महत्ता है। नृसिंह भगवान् ने प्रह्लाद के सिर पर हाथ रख कर कहा कि 'बेटा तू तो बहुत पवित्र है परन्तु अब मेरे स्पर्श से तेरे बचे-खुचे खराब संस्कार भी नष्ट हो गये हैं।' तब प्रह्लाद ने पूछा कि उसके पिता हिरण्यकश्यपु के पापों का क्या? तब भगवान् ने बतलाया कि जब उसे उनके हाथों का स्पर्श प्राप्त हो गया है तब पाप तो बच ही कैसे सकते हैं। उसका तो परम् कल्याण हो ही गया। यह एक प्रतीकात्मक कथा के रूप में समझाने का प्रयास है कि भगवान् के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हो जाने पर फिर क्या बाकी रह गया? हमारी भारतीय पौराणिक परंपरा में भगवान् के स्पर्श को बड़ा भारी महत्त्व प्रदान किया जाता है। उनके स्पर्श मात्र से दुष्ट से दुष्ट पापियों और असुरों का भी तत्क्षण कल्याण हो जाता है। और वास्तव में बात ऐसी ही है।
यही श्रीमाताजी ने श्रीअरविन्द के विषय में कहा था कि "विश्व के इतिहास में श्रीअरविन्द जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं वह कोई शिक्षा नहीं है, कोई अंतःप्रकटन भी नहीं है, वह तो परमोच्च से आती एक निर्णायक क्रिया है।"* और वह क्रिया निष्फल नहीं हो सकती। इस बात का हमें अब पूरा आभास और आश्वासन है कि वे अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे अपितु अवश्य ही उसे उसकी पूर्णाहुति तक पहुँचाएँगे। इस पृथ्वी की लाखों वर्षों से चली आ रही जो पीड़ाएँ हैं उनका निर्णायक रूप से समाधान किया जाएगा। इस कार्य में सारे देवता आदि सभी सहयोग के लिये तैयार हैं। पर जितना कार्य श्रीमाताजी ने कर लिया उससे आगे बढ़ने पर ही यह संसिद्ध हो सकता है अन्यथा नहीं। और यह कार्य स्वयं श्रीमाताजी ही कर सकती हैं, उनके अतिरिक्त और कौन कर सकता है? परंतु यह निश्चित है कि वे अपनी क्रिया करेंगी और अपने कार्य को संसिद्ध करेंगी। हालाँकि किन साधनों से और किस तरीके से वे ऐसा करेंगी ये सब चीजें तो संकीर्ण मानवीय बुद्धि की समझ से परे हैं।
सिस्टर निवेदिता ने एक स्थान पर लिखा है कि जब शारदा माँ के पास बैठ कर वे ध्यान कर रही थीं तब एकाएक ही उन्हें अपनी मूर्खता का भान हुआ कि जब स्वयं जगदंबा उनके निकट बैठी हैं तो वे अन्य किसका ध्यान लगा रही हैं। उस समय शारदानंद जी और ब्रम्हानंद जी ही आश्रम की व्यवस्था सम्भालने वाले मुख्य व्यक्तियों में से थे। शारदानंदजी बड़े ही समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने शारदा माँ की ड्योढ़ी सम्भालने का कार्य लिया। वास्तव में करने का काम तो केवल यही है। भगवान् की पादुका साफ करने से, उनकी सेवा करने से ही व्यक्ति का रास्ता सच्चे रूप में बैठ सकता है। पर यह बात तो किसी समझदार व्यक्ति को ही समझ में आ सकती है जैसे कि शारदानंद जी को समझ में आ गई। शारदा माँ और श्रीरामकृष्ण परमहंस अभी भी विद्यमान हैं और पूरी तरह सक्रिय हैं। और श्रीअरविन्द ने कहा है कि श्रीरामकृष्ण परमहंस ने स्वयं सूक्ष्म शरीर में आकर उन्हें योग साधना में दीक्षित किया था।
* (CWM * 13, 4)
प्रश्न : अवतार जो बाहरी यंत्र काम में लेते हैं क्या उसका कोई अंश जैसे मन, प्राण अथवा शरीर का कोई भाग आगे भी बचा रहता है?
उत्तर : उनकी देह तो चिन्मय है। उनकी पूरी सत्ता चैत्यमय है
इसलिए वह नाशवान् नहीं होती। भौतिक शरीर के अतिरिक्त अन्य सभी भाग तो रूपांतरित रहते हैं। इसलिये वे नष्ट नहीं होते। इसीलिये वे इस पार्थिव जगत् के निकट रह कर अपनी क्रिया कर सकते हैं। श्रीअरविन्द तो हमारे इस जगत् के बिल्कुल निकट सूक्ष्म भौतिक जगत् में ही विद्यमान हैं। और शारदा माँ और श्री रामकृष्ण जी भी यहीं हैं। श्रीरामकृष्णजी के बारे में तो श्रीअरविन्द ने कहा था कि उनमें इतनी पवित्रता थी कि उन्हें तो रूपांतरण की भी आवश्यकता नहीं थी। हम देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का भी जगत् में कितना भारी प्रभाव है।
प्रश्न : अवतार रूप में जन्म से पूर्व अवतारों की पूर्वजन्मों में तैयारी हुई होती है?
उत्तर : हो सकता है कि तैयारी हो, और संभव है कि न भी हो। इसका कोई तय नियम नहीं है। श्रीमाताजी की सत्ता की तो बहुत तैयारियाँ की गईं थीं। श्रीअरविन्द ने कहा कि उनकी हजारों वर्षों से तैयारी हुई है। और वे ऐसे विशेष तत्त्वों को लेकर आविर्भूत हुईं थीं कि वे जन्म से ही मुक्त थीं और मनुष्यता से ऊपर थीं। श्रीमाताजी को सुदीर्घ काल से विकसित सत्ता प्राप्त हुई थी अन्यथा यदि बाहरी सत्ता की तैयारी में उनका समय लग जाता तब फिर जो विशेष कार्य पृथ्वी पर उन्हें करना था वह तो उनके लिए संभव ही नहीं हो पाता। इन रहस्यों का श्रीअरविन्द व श्रीमाँ ने अपने पत्रों के माध्यम से उद्घाटन किया है जिस कारण इनके विषय में हमें इतनी जानकारी प्राप्त हो सकी है।
महामनस्वी और वीरतापूर्ण व्यक्तित्वों को देवतातुल्य बनाने की स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति के मूल में यही सत्य है। यह प्रवृत्ति भारतीय मन की इस आदत से पर्याप्त सुस्पष्टता से सामने आती है जो सहज ही महान् संत-महात्माओं, आचार्यों और पंथ-प्रवर्तकों में अंश-अवतार देखती है, या फिर यह प्रवृत्ति दक्षिण के वैष्णवों के इस दृढ़ विश्वास में अत्यंत प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है कि उनके कुछ संत भगवान् विष्णु के प्रतीकात्मक सचेतन आयुधों के अवतार हैं, क्योंकि सचमुच सभी महान् आत्माएँ यही तो हैं- भगवान् की सचेतन शक्तियाँ और आयुध, जिन्हें ऊर्ध्वगामी प्रयाण में और (उसमें प्रस्तुत होने वाली विघ्न-बाधाओं से) संग्राम में युद्ध करने के काम में लिया जाता है। यह भाव जीवन के विषय में किसी भी रहस्यवादी या आध्यात्मिक दृष्टि के लिए - जो भगवान् की सत्ता और उनकी प्रकृति तथा मानवसत्ता और उसकी प्रकृति के बीच अमिट रेखा नहीं खींचती सहज और अपरिहार्य है, यह मानवता में भगवान् का बोध है। परन्तु फिर भी विभूति अवतार नहीं हैं, अन्यथा अर्जुन, व्यास, उशना भी सब वैसे ही अवतार होते जैसे श्रीकृष्ण थे, चाहे उनमें अवतारपन की शक्ति इनसे कुछ कम ही होती। केवल दिव्य गुण का होना ही पर्याप्त नहीं है; उन परमेश्वर और परमात्मा की आंतरिक चेतना का होना भी आवश्यक है जो अपनी दिव्य उपस्थिति से मानव-प्रकृति का संचालन करते हैं। गुणों की शक्ति का उन्नयन अभिव्यक्ति (भूतग्राम) का ही ix8 अंग है, सामान्य अभिव्यक्ति में यह ऊर्ध्व-आरोहण है। परंतु अवतार में एक विशेष अभिव्यक्ति होती है, यह दिव्य जन्म ऊपर से होता है, सनातन विश्वव्यापक देव व्यष्टिगत मानवता के एक आकार में उतर आते हैं 'आत्मानं सृजामि' और वे प्रच्छन्न रूप से निज-स्वरूप के विषय में सचेतन आवरण के पीछे ही नहीं होते, अपितु बाह्य प्रकृति में भी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है।
विभूति को अपने विषय में ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है, परन्तु अवतार को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। भगवान् और उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनके जो आयुध हैं वे भी अवतार तथा अंशावतार के रूप में आविर्भूत होते हैं जिनमें इतनी शक्ति होती है जो बाधाओं को दूर कर के पार्थिव अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जी लक्ष्मणजी के तथा यमुनाचार्य जी भगवान् के सिंहासन के अवतार माने जाते हैं। विभिन्न आळ्वार भगवान् के शंख, चक्र, गदा, खड्ग, आदि के अवतारों के रूप में आविर्भूत हुए हैं। आण्डाळ को महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं। ऐसे ही किसी को कौस्तुभ मणि का तो अन्य किसी को किसी अन्य आयुध का अवतार माना जाता है। दक्षिण में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में ही हम भगवान् के ऐसे विशिष्ट आविर्भावों, विशिष्ट शक्तियों और विशिष्ट विभूतियों के आविर्भाव का वर्णन पाते हैं। इन लोगों के आविर्भाव में ऐसी शक्ति होती है कि ये जीवन को बिल्कुल मोड़ कर, उसकी दिशा सर्वथा बदल कर चले जाते हैं। अन्यथा तो मनुष्य अपनी ही प्रकृति से जीवन भर संघर्ष करता रहता है और इससे अधिक कुछ कर ही नहीं पाता। अतः इन विभूतियों आदि के रूप में भगवान् की विशिष्ट शक्ति आविर्भूत होती है, और उस विशिष्ट शक्ति के कारण ही वे पार्थिव प्रकृति और चेतना पर अपना आधिपत्य जमा पाते हैं अन्यथा सामान्य मानव चेतना से तो ऐसा करना संभव ही नहीं है।
हालाँकि ये सब विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ भी आवश्यक रूप से अवतार के लक्षण नहीं हैं। अवतार के लिए तो मूलभूत रूप से यह सज्ञानता और चेतना होनी आवश्यक है कि वह स्वयं भगवान् ही है। हालाँकि भगवान् का अंश तो सभी में होता है परन्तु अवतार को अपनी बाहरी प्रकृति में भी इस बात का बोध और पूरा ज्ञान होता है कि वह स्वयं परमात्मा ही है। भगवान् श्रीराम को भी अपने अवतार होने का पूरा ज्ञान था हालाँकि उन्होंने कभी ऐसा प्रकट नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में भी हमें यह पता चलता है कि भगवान् श्रीराम अपने इस तत्त्व को जानते थे। अध्यात्म रामायण में तो प्रकट रूप से है ही कि वे अवतार थे। श्रीकृष्ण ने भी उचित समय पर ही अर्जुन के समक्ष अपना निज-स्वरूप प्रकट किया। अतः अवतार का यह एक विशिष्ट लक्षण है कि उसे अपने अवतार होने का आभास आरंभ से ही होता है, और धीरे-धीरे यह आभास अधिक स्पष्ट होता जाता है और बिल्कुल निश्चित हो जाता है। परंतु अपने विषय में श्रीअरविन्द ने कहा कि उन्हें इसका कोई स्पष्ट भान नहीं था, बस इतना अवश्य आभास था कि उन्हें इस राष्ट्र के लिए कुछ विशेष कार्य करना है।
प्रश्न : श्रीअरविन्द को यह अहसास कब हुआ कि वे अवतार हैं?
उत्तर : उन्होंने कभी ऐसी घोषणा नहीं की और न स्वयं को अवतार बताया। परन्तु श्रीमाँ ने श्रीअरविन्द के विषय में भी अवतार होने की बात कही थी और स्वयं के विषय में भी यह कहा कि वे स्वयं जगदम्बा हैं जो सचेतन रूप से भागवत् कार्य हेतु अवतरित हुईं हैं। श्रीअरविन्द आश्रम पांडिचेरी की ही एक साधिका सहाना देवी अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि आश्रम में आने के कुछ महीनों बाद ही जब उन्हें इस बात को लेकर गहरी बेचैनी हुई कि जिन श्रीकृष्ण के नाम और भजनों को लेकर वे पहले द्रवित हो जाया करती थीं और उनके प्रेमाश्रु बहने लगते थे वह स्थिति अब धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही थी और उनके स्थान पर उनके हृदय में भावनाएँ श्रीमाँ व श्रीअरविन्द के चारों ओर केंद्रित होती जा रही थीं। जब वे इस बात को लेकर लंबे समय तक गहरी कशमकश में थीं तब एक दिन उन्हें एक गहरा अनुभव हुआ जिसमें श्रीकृष्ण ने आकर उनसे कहा कि, "यह उदासी क्यों? मैं श्रीअरविन्द के साथ संयुक्त हूँ।" जब उन्होंने अपने इस अनुभव को श्रीअरविन्द को लिखकर बताया और इसका अर्थ पूछा तो श्रीअरविन्द ने इस बात की पुष्टि की कि "श्रीकृष्ण के अतिरिक्त मेरे साथ और कौन संयुक्त हो सकता है?"*
इसी प्रकार २ मार्च १९३२ को जब एक साधक ने अपने पत्र में लिखा कि, "अब से पहले तक मैंने श्रीकृष्ण के अतिरिक्त किसी की भी भगवत्ता को स्वीकार नहीं किया था। मैंने श्रीमाँ को एक गुरु के रूप में देखा है जो मुझे उन तक ले जा सकती हैं।
----------------
At the feet of the Mother and Sri Aurobindo by Sahana, (ed. 1985) p. 230
परंतु अब मेरे अंदर एक ऐसी चीज है जो श्रीमाँ को दृढ़ रूप से भगवत् शक्ति के रूप में मानना चाहती है। मैं उन्हें मन से दूर नहीं रख पाता और न ही श्रीकृष्ण को अस्वीकार कर पाता हूँ। जितना ही मैं इस विषय में सोचता हूँ उतना ही असमंजस में पड़ता जाता हूँ। मैं आपकी सहायता की प्रार्थना करता हूँ।" तो इसके उत्तर में श्रीअरविन्द ने लिखा कि, "तुम्हारे अंदर का यह संघर्ष सर्वथा अनावश्यक है; क्योंकि दोनों चीजें एक ही हैं और बिल्कुल समुचित रूप से एक-दूसरे के साथ सुसमंजस हैं। वे ही तुम्हें श्रीमाँ के पास लाए हैं और श्रीमाँ की पूजा-भक्ति के द्वारा तुम उनका (श्रीकृष्ण का) साक्षात्कार कर सकते हो। वे (श्रीकृष्ण) यहाँ आश्रम में हैं और उन्हीं का कार्य यहाँ किया जा रहा है।" (CWSA 32, p.337)
प्रश्न : यों तो श्रीमाँ ने श्रीअरविन्द से २९ मार्च १९१४ को हुई भेंट के बाद ही घोषणा कर दी थी कि "जिन्हें हमने कल देखा था वे पृथ्वी पर विद्यमान हैं।" (CWM 13, p.3)
उत्तर : उस समय उन्होंने श्रीअरविन्द को अवतार के रूप में घोषित नहीं किया था। उन्होंने केवल यही कहा कि उनकी उपस्थिति से पृथ्वी पर कुछ निर्णायक होने वाला है।
एक मध्यवर्ती विचार भी है, अवतार के विषय में एक अधिक रहस्यवारी दृष्टिकोण जिसके अनुसार एक मानव-आत्मा अपने अन्दर भगवान् का आदान कर के यह अवतरण साधित कराती है और तब वह भागवत् चेतना के अधिकार में हो जाती है अथवा उसका प्रभावशाली प्रतिबिंब या माध्यम बन जाती है। यह दृष्टिकोण आध्यात्मिक अनुभव के कुछ विशिष्ट सत्यों पर आश्रित है। मनुष्य में दिव्य जन्म, मनुष्य का आरोहण अपने-आप में मानव-चेतना का भागवत् चेतना में संवर्द्धन है, और अपनी प्रगाढ़तम परिणति में पृथक् आत्मा का उस भागवत् चेतना में लय हो जाना है.. स्वयं गीता जीव के ब्रह्मभूत हो जाने और उसी कारण भगवान् में, श्रीकृष्ण में निवास करने की बात कहती है, परंतु यह ध्यान में रहे कि गीता इस जीव के भगवान या पुरुषोत्तम हो जाने के बारे में कहीं नहीं कहती। भले ही, जीव के संबंध में गीता इतना अवश्य कहती है कि जीव सदा ही ईश्वर है, भगवान् की अंशसता है, ममैवांशः। क्योंकि यह महानतम मिलन, यह उच्चतम परिणति भी आरोहण का ही एक अंग है; और यद्यपि यह वह दिव्य जन्म है जिस तक प्रत्येक जीव पहुँचता है, परंतु यह परमेश्वर का नीचे उतरना नहीं है, यह अवतार नहीं है, अपितु अधिक-से-अधिक, बौद्ध मत के अनुसार इसे हम बुद्धत्व की प्राप्ति कह सकते हैं, यह जीव का अपने वर्तमान साधारण लौकिक व्यष्टिभाव से जागृत होकर अनंत परम्-चेतना को प्राप्त होना है। इसमें अवतार की आंतरिक चेतना अथवा उसकी विशिष्ट क्रिया हो यह आवश्यक नहीं है।
xvi.54
दूसरी ओर, भागवत् चेतना में इस प्रवेश की प्रतिक्रियास्वरूप भगवान् का हमारी सत्ता के मानव-अंगों में प्रवेश या उन अंगों में (सम्मुख आकर) प्राकट्य हो सकता है और मनुष्य की प्रकृति, उसके क्रियाकलाप, उसको मानसिकता और यहाँ तक कि भौतिकता में भी वे स्वयं को उँड़ेल सकते हैं; और तब वह कम-से-कम एक आंशिक अवतार हो सकता है...
अब यह एक दूसरी बात है। यह आवश्यक नहीं है कि जन्म से ही व्यक्ति अवतार रूप में जन्म ग्रहण करे। श्रीअरविन्द के अनुसार यदि किसी मनुष्य की अन्तरात्मा बहुत विकसित हो और वह साधना में आरोहण करते हुए भागवत्-चेतना तक पहुँच जाए और उससे एक हो जाए तो उसे अवतार नहीं कहेंगे। क्योंकि वह अवतरण नहीं होता बल्कि वह तो नीचे से आरोहण ही होता है। उसे कुछ हद तक भगवान् का अंश कह सकते हैं 'मम अंश सनातनः। परन्तु ऐसा भी संभव है कि उसके एक निश्चित विकास के फलस्वरूप भगवान् स्वयं उसमें अवतरित हो जाएँ और उसके कुछ हिस्सों में स्वयं को अभिव्यक्त कर दें। इसे आंशिक अवतार कहेंगे। यह तो ऊपर से अवतरित होती चेतना है जो व्यक्ति को अधिग्रहीत कर लेती है। वह अधिग्रहण होने पर कम-से-कम आंशिक अवतार तो हो ही गया। ऐसा भी हो सकता है कि वह चेतना कुछ समय के लिये अधिग्रहीत कर ले और फिर लौट जाये। श्रीचैतन्य महाप्रभु के साथ यही होता था। जब उन्हें भगवद् आवेश ने अधिग्रहीत कर लिया तब सात प्रहर तक वे उसी भाव में थे। जब वह भाव शांत हुआ तब जाकर वे पुनः अपनी सामान्य अवस्था में लौटे। अवतार में गति ऊपर से नीचे की ओर होती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। साधना में आरोहण द्वारा व्यक्ति बुद्ध जैसी स्थिति तो प्राप्त कर सकता है, परन्तु गीता जिस अवतार की बात करती है वह भिन्न है। गीता इनमें से किन्हीं भी विकल्पों के अंदर नहीं जाती। वह तो दूसरी ही बात करती है जो बड़ी ही विलक्षण है।
परन्तु यह भी संभव है कि पुरुषोत्तम की उच्चतर दिव्य चेतना मनुष्य के अन्दर उत्तर आये और जीव-चेतना का उसमें लय हो जाए। उनके समकालीन लोग बतलाते हैं कि यही बात श्रीचैतन्य के समय-समय पर देवभावारूढ़ होने में हुई, जो कि अपनी सामान्य चेतना में भगवान् के केवल एक प्रेमी और भक्त होते थे और स्वयं के सभी प्रकार के दैवीकरण को अस्वीकार करते थे, परंतु वे ही इन विलक्षण क्षणों में स्वयं भगवान् हो जाते थे और भागवत्-सत्ता के उमड़ते हुए प्रकाश, प्रेम और शक्ति से संपन्न होकर उसी भगवद्भाव में बोलते और कर्माचरण करते थे। इसी को यदि जीवन की सामान्य अवस्था मान लें, अर्थात् मनुष्य सतत् ही अन्य और कुछ न रहकर इस भागवत् सत्ता और भागवत् चेतना का एक पात्र ही बन जाए तो अवतार संबंधी इस मध्यवर्ती विचार के अनुसार यह एक अवतार ही होगा। हमारी मानवीय धारणाओं को यह सहज ही संभव प्रतीत होता है; कारण, यदि मानव अपनी प्रकृति को इतना उन्नत कर सके कि उसे भगवान् की सत्ता के साथ एकत्व अनुभव हो और वह स्वयं उस भागवत्-सत्ता की चेतना, प्रकाश, शक्ति और प्रेम का मात्र एक वाहक बन जाए, और उसका अपना संकल्प और व्यक्तित्व भगवान् के संकल्प और उनकी सत्ता में लय हो जाए और यह एक मानी हुई आध्यात्मिक स्थिति है, - तो इसमें कोई मूलभूत असंभाव्यता नहीं है कि इसकी प्रतिक्रिया के रूप में वह दिव्य संकल्प, सत्ता, शक्ति, प्रेम, प्रकाश और चेतना मानव-जीव के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिकृत कर ले। और, यह हमारे मनुष्यत्व का एक दिव्य जन्म और दिव्य स्वभाव में कोई आरोहण मात्र ही नहीं होगा अपितु दिव्य पुरुष का मानव में अवतरण, एक अवतार, भी होगा।
यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र बता रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भगवद्-भाव के प्रति सचेतन नहीं थे। उस चेतना के चले जाने पर, उस भाव की अभिव्यक्ति नहीं रहने पर भी उनके अंदर एक चेतना बनी रहती थी जो जानती थी कि वे कौन हैं। उन्होंने भक्तों को भी उनकी अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके आराध्य देव को अपने अंदर प्रकट किया। उनमें लोगों को भगवान् श्रीराम, श्रीकृष्ण तथा अन्य रूपों के दर्शन हुए। इसका अर्थ है कि यह तत्त्व उनके अंदर प्रकट था, पर आवश्यक नहीं कि वे प्रत्यक्ष रूप से उसे अभिव्यक्त करते। श्रीराम ने भी तो प्रकट नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का तो बहुत विशिष्ट प्राकट्य था जो छिपा नहीं रह सकता था। तो यह एक बीच के भाव की तरह है कि भगवान् कभी भी अवतरित हो सकते हैं। अवतरण कभी भी हो सकता है। पर गीता इन सब की बात नहीं करती, वह किसी मनुष्य की, जीव की बातें नहीं करती। यहाँ तो जीव की कोई चर्चा ही नहीं है। भगवान् कृष्ण कहते हैं कि मैं और मेरी पराप्रकृति का ही सारा कार्य व्यापार है।
हालाँकि गीता और भी बहुत आगे निकल जाती है। वह स्पष्ट रूप से भगवान् के स्वयं जन्म लेने की बात करती है; श्रीकृष्ण अपने उन बहुत से बीते हुए जन्मों के बारे में कहते हैं और अपनी भाषा से यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे केवल ग्रहणशील मानव-प्राणी में उतर आने की बात नहीं कह रहे हैं, अपितु भगवान् के ही बहुत से जन्म ग्रहण करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ वे ठीक सृष्टिकर्ता की भाषा में बोल रहे हैं, इसी भाषा का प्रयोग वे वहाँ करेंगे जहाँ अपनी जगत्-सृष्टि की बात कहेंगे। "यद्यपि मैं प्राणियों का अजन्मा ईश्वर हूँ तो भी मैं अपनी माया से अपने-आपको सृष्ट करता हूँ" – अपनी प्रकृति के कार्यों का अधिष्ठाता होकर। यहाँ ईश्वर और मानव-जीव का अथवा पिता या पुत्र का, दिव्य मनुष्य का कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल भगवान् और उनकी प्रकृति की बात है। भगवान् निज-प्रकृति के द्वारा मानव-आकार और प्रकार में उतरकर जन्म लेते हैं और भले ही वे स्वेच्छा से मनुष्य के आकार, प्रकार और साँचे के अन्दर रहकर कर्म करना स्वीकार करते हैं, तो भी उसके अन्दर भागवत् चेतना और भागवत् शक्ति को ले आते हैं और शरीर के अन्दर प्रकृति के कर्मों का नियमन वे उसकी अंतःस्थित और ऊर्ध्व-स्थित आत्मा के रूप में करते हैं, अधिष्ठाय । ऊपर से वे सदा ही शासन करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार वे समस्त प्रकृति का शासन चलाते हैं, जिसमें मनुष्य-प्रकृति भी सम्मिलित है; अन्दर से भी वे समस्त प्रकृति का शासन करते हैं, किन्तु प्रच्छन्न रहते हुए; अंतर यह है कि अवतार में वे प्रकट या अभिव्यक्त रहते हैं, और यह कि प्रकृति ईश्वर, अंतर्यामी पुरुष, के रूप में भागवत् उपस्थिति के विषय में सचेतन रहती है, और यहाँ प्रकृति का संचालन ऊपर से उनकी गुप्त इच्छा के द्वारा 'स्वर्ग में स्थित पिता के संकल्प के द्वारा' नहीं होता, अपितु भगवान् अपने सर्वथा सीधे और प्रकट संकल्प के द्वारा प्रकृति का संचालन करते हैं। यहाँ किसी मानव मध्यस्थ के लिये कोई स्थान नहीं दिखाई देता; क्योंकि यहाँ 'भूतानां ईश्वर' स्वयं अपनी प्रकृति, प्रकृतिं स्वां, का आश्रय लेकर, न कि किसी जीव की विशिष्ट प्रकृति का आश्रय लेकर, इस प्रकार मानव-जन्म धारण कर लेते हैं।
यह सिद्धांत बड़ा ही मुश्किल है, मनुष्य की तर्कबुद्धि के लिए इसे स्वीकार कर लेना कठिन है; जिसका कारण भी स्पष्ट है, वह है प्रत्यक्षतः अवतार का मनुष्य-सदृश दिखाई देना। अवतार सदा ही भगवत्ता और मनुष्यता का द्विविध विषय होता है; भगवान् मानव प्रकृति को, उसकी सभी बाहरी सीमाओं सहित अपने ऊपर धारण करते हैं और उन सीमाओं को भागवत् चेतना और भागवत् शक्ति की अवस्थाएँ, उसके साधन और उपकरण तथा दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का एक पात्र बना लेते हैं। परंतु ऐसा ही होना भी चाहिए; क्योंकि अन्यथा अवतार के अवतरण का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होता; क्योंकि वह उद्देश्य यही दिखलाना है कि अपनी सभी सीमाओं के रहते भी मानव-जन्म दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का ऐसा ही एक साधन और उपकरण बनाया जा सकता है, ठीक यह दिखलाने के लिए कि मूर्तिमान या अभिव्यक्त चेतना के दिव्य सारतत्त्व के साथ मानव-चेतना का मेल बैठाया जा सकता है, मानव चेतना को दिव्य चेतना के पात्र में बदला जा सकता है, और उसके साँचे को रूपांतरित कर के उसकी प्रकाश, प्रेम, सामर्थ्य और पवित्रता की शक्तियों को ऊपर उठाकर उसे दिव्य चेतना के घनिष्ठ रूप से सदृश बनाया जा सकता है; और यह दिखाने के लिए भी कि यह कैसे किया जा सकता है। यदि अवतार को सर्वथा अलौकिक रूप से कार्य करना होता, तो इससे इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। एक महज अलौकिक और चमत्कारपूर्ण अवतार तो एक निरर्थक विसंगति होगी; ऐसा नहीं है कि अलौकिक शक्तियों के प्रयोग का सर्वथा अभाव हो जैसे कि ईसा द्वारा रोगियों को स्वस्थ कर देनेवाले तथाकथित चमत्कार रहे हैं, क्योंकि अलौकिक शक्तियों का प्रयोग मानव-प्रकृति के लिए बहुत कुछ संभव है; परन्तु अवतार में इन अलौकिक शक्तियों का लेशमात्र भी हो यह आवश्यक नहीं, और न ही यह किसी भी हाल में पूरे विषय का कोई मूल तत्त्व ही है, और इससे भी कुछ सिद्ध नहीं होगा यदि अवतार का जीवन और कुछ नहीं केवल विलक्षण आतिशबाजियों का प्रदर्शनमात्र हो। अवतार कोई ऐंद्रजालिक जादूगर के रूप में नहीं आते, अपितु मनुष्य-जाति के दिव्य नेता और दिव्य मनुष्यत्व के प्रतिमान या दृष्टांत के रूप में आते हैं। यहाँ तक कि उन्हें मानवीय शोक और भौतिक यंत्रणा भी अवश्य ही झेलनी पड़ती हैं और उनसे काम लेना पड़ता है, ताकि यह दिखला सकें कि, सर्वप्रथम, किस प्रकार वह शोक और यंत्रणा आत्मोद्धार का एक साधन हो सकता है, जैसा कि ईसा ने किया, और, दूसरे, यह दिखाने के लिए कि मानव-प्रकृति में अवतरित दिव्य आत्मा द्वारा इस शोक और यंत्रणा को स्वीकार कर के उसी प्रकृति में उसे जीता भी जा सकता है - जैसा कि बुद्ध ने किया।
--------------------------
* यदि भगवान् मूलतः सर्वशक्तिमान् न होते तो वे कहीं भी सर्वशक्तिमान् न होते... चूंकि वे अपने कार्य को अवस्थाओं के द्वारा सीमित या निर्धारित करना पसंद करते हैं तो इससे वे कुछ कम सर्वशक्तिशाली नहीं बन जाते। स्वयं उनका आत्म-सीमन भी सर्वशक्तिमत्ता का ही एक कृत्य है....
भला भगवान् को अपनी सभी क्रियाओं में सफल होने के लिये ही क्यों बँधे रहना चाहिये? यदि विफलता उन्हें अधिक अनुकूल पड़ती हो और उनके अंतिम हेतु को सिद्ध करने में अधिक सहायक होती हो तो? भगवान् के विषय में कैसे सख्त अशिष्ट विचार हैं ये! लीला के लिये कुछ विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं और जबतक वे अवस्थाएँ अपरिवर्तित बनी रहती हैं, कुछ चीजें नहीं की जा सकतीं, इसलिए हम कहते हैं कि वे असंभव हैं, नहीं की जा सकतीं। यदि अवस्थाओं को बदल दिया जाए तो वे ही (असंभव प्रतीत होने वाली) चीजें की जाती हैं या कम-से-कम करने योग्य बन जाती हैं - प्रकृति के तथाकथित नियमों के अनुसार न्यायसंगत, स्वीकार्य बन जाती हैं और तब हम कहते हैं कि वे की जा सकती हैं। भगवान् भी लीला की शर्तों के अनुसार कार्य करते हैं। वे उन्हें बदल सकते हैं, परंतु पहले उन्हें उन शर्तों या नियमों को बदलना होता है, न कि उन नियमों को बनाये रखते हुए ही चमत्कारों की एक श्रृंखला के द्वारा कार्य करने में प्रवृत्त हो जाते हैं।
एक अवतार या विभूति को उतना ज्ञान होता है जितना उनके कार्य के लिए आवश्यक हो, उससे अधिक होना उनके लिए आवश्यक नहीं। इस बात का सर्वथा कोई कारण नहीं कि बुद्ध को यह क्यों जानना चाहिए कि रोम में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि एक अवतार भगवान् की संपूर्ण सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमत्ता भी अभिव्यक्त नहीं करता; वह ऐसे कोई अनावश्यक प्रदर्शन के लिए नहीं आता; यह सब उसको चेतना में निहित अवश्य होता है परंतु उसकी चेतना के अग्रभाग में नहीं होता। जहाँ तक विभूति की बात है, उसे तो संभवतः यह भी पता न हो कि वह भगवान् की एक शक्ति है।
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ।। ९।।
९. हे अर्जुन ! जो मनुष्य मेरे इस प्रकार के दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थ रूप में जानता है वह मनुष्य देह परित्याग करने पर दूसरी बार जन्म को नहीं प्राप्त होता अपितु मुझे प्राप्त होता है।
जिस कर्म के लिए अवतार अवतरित होता है उसका भी उसके जन्म की ही भाँति द्विविध भाव और द्विविध रूप होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया के जिस विधान के द्वारा, उत्थान और पतनरूपी जिस व्यवस्था के द्वारा प्रकृति अग्रसर होती है, उस विधान और व्यवस्था के होते हुए भी दिव्य विधान की रक्षा और पुनर्गठन के लिए इस बाह्य जगत् पर भागवत् शक्ति की जो क्रिया होती है, वही दिव्य कर्म का बाह्य पहलू है, और इस दिव्य विधान द्वारा हो मानव जाति के भगवन्मुख प्रयास की किसी भयंकर प्रत्यावर्तन से रक्षा की जाती है, अपितु उसकी अपेक्षा उसे निर्णायक रूप से आगे की ओर ले जाया जाता है। इसका एक आंतरिक पहलू है जिसमें भगवन्मुख चेतना की दिव्य शक्ति व्यक्ति और जाति की आत्मा पर क्रिया करती है ताकि वह मानवरूप में अवतरित भगवान् के प्रकटन के नवीन रूपों को ग्रहण कर सके और अपने ऊर्ध्वमुखी आत्म-विकास या आत्मोद्घाटन की शक्ति को बनाये रख सके, उसमें एक नवजीवन ला सके और उसे समृद्ध कर सके। अवतार मात्र किसी महान् बाह्य कर्म के लिए अवतरित नहीं होता, जैसा कि मनुष्य की कर्म-प्रवण बुद्धि प्रायः ही मानने को उद्यत रहती है।...
जिस संकटकाल में अवतार का आविर्भाव होता है, जो यद्यपि बहिर्मुखी दृष्टि को महज घटनाओं और भीषण भौतिक परिवर्तनों के संकट के रूप में गोचर होता है, परंतु वह सदा ही अपने मूलस्रोत और यथार्थ अर्थ में मानवजाति की चेतना के ऐसे दौर में उपस्थित हुआ एक संकटकाल होता है जब उसे किसी अतिविशाल रूपांतर से गुजरना होता है और कोई नवीन विकास चरितार्थ करना होता है। इस परिवर्तन की क्रिया के लिये किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती है; परन्तु वह शक्ति जिस चेतना को धारण करती है सदा उसके बल के अनुरूप निर्धारित होती है; इसीलिए मानवजाति के मन और अंतरात्मा में भागवत् चेतना के आविर्भाव की आवश्यकता होती है। अवश्य ही, जहाँ परिवर्तन मुख्यतः बौद्धिक और व्यावहारिक हो, वहाँ अवतार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती; मानव-चेतना का एक महत् उत्थान होता है, शक्ति की एक महान् अभिव्यक्ति होती
---------
* जो स्वर्गों को इस धरा पर लाएगा, उसे स्वयं उतरना होगा पंक भीतर और होगा झेलना पार्थिव प्रकृति के बोझ को, और चलना होगा कष्टपूर्ण पथ ऊपर ।। अपने देवत्व को दबाकर, आया मैं, नीचे इस पतित घरा ऊपर
अज्ञानमय, श्रमरत, मानव बना, मृत्यु व जन्म के द्वारों के मध्य होकर।। खोद रहा मैं लंबी-गहरी, मलिनता और दलदल के भीतर
स्वर्णिम सरिता के गान को एक नहर, अमर ज्वाला हेतु एक घर ।।
जड़ता की रात्रि में मैंने श्रम किया है, दुःख सहा है, लाने को अग्नि मनुष्य के पास पर नरक की घृणा और मानव विद्वेष, जगत् के आरंभ से रहे मेरे पुरस्कार।।
...खुले पड़े मेरे घाव सहस्र, और असुर राजा करते वार पर रुक न सकता मैं परिणति तक, जबतक न हो जाता शाश्वत संकल्प साकार।।
एक हताश पथ पर पड़े हैं मेरे चरण, निःसीम शांति से ढके हुए देव वैभव की अग्नियों को, जो ले आते मानव रसातल में ।।
-भगवान् का श्रम
* पीछे परिशिष्ट देखें
है जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए मनुष्य अपनी साधारण अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं, और चेतना और शक्ति की यह तरंग किन्हीं असाधारण व्यक्तियों, विभूतियों, में अपना चरम उत्कर्ष पाती है जिनकी क्रिया द्वारा सामान्य मानव जाति के कर्म का नेतृत्व किया जाना ही अभीष्ट परिवर्तन के लिये पर्याप्त होता है। यूरोप में पुनर्निर्माण और फ्रांसीसी क्रांति इसी प्रकार के संकटकाल थे... परंतु जब किसी संकट के मूल में कोई आध्यात्मिक बीज या हेतु निहित होता है तब भागवत्-चेतना के प्रवर्तक या नेता के रूप में एक मानव-मन और आत्मा में देव-चेतना का एक पूर्ण या आंशिक प्रादुर्भाव होता है। यही अवतार है..."
अवतार के आने का मुख्य कारण है कि समय-समय पर मनुष्य अपनी सीमाओं में बंध जाते हैं और उन्हीं घेरों में चक्कर काटते रहते हैं और भगवान् की उत्तरोत्तर होती आत्म-अभिव्यक्ति को आसानी से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए अवतार अपनी उपस्थिति की शक्ति द्वारा पूरे समीकरण में अंतर ले आते हैं और मनुष्य को इन सीमाओं से निकालने में सहायता करते हैं ताकि वे उत्तरोत्तर होती आत्म-अभिव्यक्ति में आगे बढ़ सकें। उदाहरण के लिए जब भगवान् श्रीराम का प्रादुर्भाव हुआ उस समय बहुत अराजकता फैली हुई थी। धर्म का पालन भी समुचित रूप से नहीं हो रहा था। ऐसे में भगवान् ने अवतार लेकर यह स्थापित किया कि यह अराजकता उचित नहीं है। इसकी बजाय नैतिकता के विधान का पृथ्वी पर राज्य होना चाहिये क्योंकि प्राण की अराजकता भगवान् की अभिव्यक्ति में बाधक है। उन्होंने लक्ष्मणजी, भरतजी, सीताजी आदि के आदर्श को सबके सम्मुख प्रस्तुत किया ताकि मनुष्य उनसे प्रेरणा लेकर केवल घोर स्वार्थ में ही न डूबे रहें बल्कि आपसी प्रेम और समर्पण का भाव अपना सकें और पृथ्वी पर धर्म के अनुसार जीवन यापन कर सकें।
परन्तु ये सब चीजें भगवान् की अभिव्यक्ति की कोई चरम चीजें नहीं हैं। इसलिए उनके बाद श्रीकृष्ण आए और उन्होंने नैतिक आदशों के उस पूरे दायरे को तोड़ दिया और क्योंकि वे तो दिव्य हैं और उनकी लीलाएँ दिव्य हैं इसलिए उन्हें मानसिक आदर्शों से बँधने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने भगवान् और उनके अंतरंग लोगों के बीच प्रेम-संबंध को स्थापित किया। इसमें मानवीय आदर्शों का और उसकी नैतिकता का कोई विषय ही नहीं है। आदर्श आदि सब चीजें तो अपने स्थान पर सही हैं परन्तु प्रेम का यह विधान उससे भी अधिक उच्च तत्त्व है। इसीलिए भागवत् धर्म, वृन्दावन का धर्म तो अयोध्या के धर्म से मेल नहीं खाता। ऐसा नहीं है कि वृंदावन की अभिव्यक्ति के समय अयोध्या के समय के वे सब तत्त्व विलुप्त हो गए हों बल्कि उनमें एक नया तत्त्व और जुड़ गया और मनुष्य के लिए एक नया आयाम और खोल दिया गया।
-------------------
* मोटे तौर पर कहें तो, अवतार वह है जो अपने अंदर जन्म ग्रहण किये हुए या अपने अंदर अवतरित हुए तथा भीतर से अपने संकल्प, जीवन और कर्म को संचालित करते हुए भगवान् की उपस्थिति और शक्ति के विषय में सचेतन होता है, वह अपने भीतर इस भागवत् उपस्थिति और शक्ति के साथ तादात्म्य अनुभव करता है। विभूति के विषय में यह माना जाता है कि वह भगवान् की किसी शक्ति को अभिव्यक्त करता है और उसके द्वारा जगत् में प्रचण्ड शक्ति-प्रभाव के साथ कार्य करने में समर्थ होता है; पर इतना ही उसे विभूति बनाने के लिये आवश्यक होता हैः उसको शक्ति अत्यधिक महान् हो सकती है, पर उसमें एक सहज या अंतःस्थ देवत्व की चेतना नहीं होती। यही भेद हम गीता से प्राप्त कर सकते हैं जो कि इस विषय पर प्रमुख प्रामाणिक ग्रंथ है। यदि हम इस भेद को स्वीकार करें तो हम दृढ़तापूर्वक यह कह सकते हैं कि उनका जो कुछ वर्णन हमें प्राप्त है उसके आधार पर राम और कृष्ण को अवतार माना जा सकता है। बुद्ध भी वैसे ही प्रतीत होते हैं यद्यपि उनके अंदर शक्ति की कहीं अधिक निर्व्यक्तिक चेतना ही विद्यमान थी। रामकृष्ण ने भी उसी चेतना को अभिव्यक्ति दी थी जब उन्होंने स्वयं अपने अंदर उसी 'दिव्य पुरुष' की विद्यमानता के बारे में कहा जो 'दिव्य पुरुष' राम और कृष्ण बना था। परंतु चैतन्य का प्रकरण तो विलक्षण है; क्योंकि उपलब्ध वर्णनों के अनुसार वे साधारणतया अपने को कृष्ण का एक भक्त अनुभव करते और वही बताते थे, उससे अधिक कुछ नहीं, परंतु महान् क्षणों में वे कृष्ण को अभिव्यक्त करते थे, अपने मन और शरीर में ज्योतिर्मय हो उठते थे तथा स्वयं कृष्ण बन जाते थे, भगवान् की तरह ही बोलते और कार्य करते थे। उनके समसामयिक लोगों ने उनके अंदर कृष्ण के अवतार को, भागवत् प्रेम की अभिव्यक्ति को अनुभव किया।
शंकर और विवेकानंद, निश्चय ही केवल विभूति ही थे; उन्हें इससे अधिक कुछ नहीं माना जा सकता, यद्यपि विभूतियों के रूप में वे बहुत महान् थे।
अब हमारे समय में श्रीमाँ व श्रीअरविन्द आए हैं और उन्होंने एक और भी महत् आयाम जोड़ दिया है कि भगवान् की लीला केवल मानसिक चेतना में ही अनुभव नहीं की जा सकती अपितु मानसिक चेतना से ऊपर की चेतना में भी मनुष्य जा सकता है और मृत्यु और अज्ञान को समाप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्ण इस आयाम को नहीं खोल सकते थे। परंतु यह इस पर निर्भर करता है कि मनुष्य का तात्कालिक विकास किस स्तर तक का है उसी के अनुसार उसके समक्ष कोई नया आयाम या उसकी प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ा जाता है। इसलिए श्रीराम एक पहलू को सामने लाए, श्रीकृष्ण दूसरे पहलू को सामने लाए और श्रीअरविन्द व श्रीमाँ ने इस विकासक्रम में अतिमानस के तत्त्व को जोड़ दिया। श्रीमाताजी के अनुसार अतिमानसिक चेतना के आने के बाद फिर शायद अवतारों की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः इस पूरी अवतार श्रृंखला से यह तो स्पष्ट है कि किस प्रकार इन्होंने विकास के अंदर सदा ही नए आयाम जोड़े हैं। ये नये आयाम किसी महापुरुष या महानायक के आने से नहीं जुड़ सकते। शक्ति-सामर्थ्य तो बहुतों में हो सकती है परंतु जो कार्य श्रीकृष्ण ने किया वह तो कोई सोच भी नहीं सकता भले वह कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो। यह तो केवल भगवान् का व्यक्तित्व ही है जो इन नए तत्त्वों को अभिव्यक्ति में ला सकता है। यदि श्रीअरविन्द मौजूद नहीं होते तो कोरे सिद्धान्तों से अतिमानसिक चेतना को तथा पार्थिव प्रकृति में हुए महत् परिवर्तन को नहीं लाया जा सकता था। कोरी दार्शनिक बातों से यह नहीं हो सकता। इसीलिए श्रीअरविन्द ने स्वयं प्रकट होकर अपनी उपस्थिति से इस काम को किया और दूसरों को इसकी ओर जाने का मार्ग दिखाया। साथ ही धरती पर एक ऐसी दिव्य चीज को प्रकट किया और उसे मनुष्यजाति की आत्मा में स्थापित कर दिया जिसकी कि कल्पना तक नहीं की जा सकती।
इस तरह यह स्पष्ट है कि अवतार पृथ्वी पर उत्तरोत्तर प्रगतिशील अभिव्यक्ति में नवीन तत्त्व जोड़ते हैं। श्रीकृष्ण ने उस समय मनुष्य की आत्मा में जो चीज स्थापित की वह कितने वर्षों बाद जाकर भागवत् धर्म के रूप में विकसित हुई। वैसे ही श्रीअरविन्द ने तो इस नवीन तत्त्व को मानवजाति की आत्मा में अभी हाल में ही रखा है। जब यह अपने पूर्ण प्रकाश में आएगा तभी हम इसके वास्तविक महत्त्व को समझ पाएँगे। परन्तु अवश्य ही ये चीजें मानवजाति की आत्मा में स्थापित कर दी गई हैं और इनका प्रभाव और क्रिया अमोघ है, वह रुक नहीं सकती, इसलिए निश्चित रूप से इसकी अभिव्यक्ति होगी। चूंकि भगवान् के द्वारा ही यह नवीन अभिव्यक्ति अभिप्रेत थी इसलिए इसे कोई नहीं रोक सकता।
यदि इस तरीके से हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि भगवान् तो अनंत हैं, असीम हैं। इसीलिए अवतार शरीर धारण कर के वे हमें उन अनंत की झलक प्रदान करते हैं ताकि हम चेतना के जिन किन्हीं स्तरों पर फँस जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं वहाँ से अपनी यात्रा को आगे की ओर ले जा सकें। चेतना के किसी स्तर पर फँस जाने को ही चेतना की संकटावस्था कहते हैं। मनुष्य चेतना के अमुक स्तर पर बंध जाता है, उसके आगे की सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता और अपने-आप को निस्सहाय अनुभव करता है। सभी पुराणों की रचना के बाद भी जब वेदव्यास जी को असंतोष हो रहा था तब उन्हें यह पता चला कि वास्तविक चीज तो अभी करनी बाकी ही है। यदि श्रीकृष्ण की लीला को केंद्र में रखकर कोई कृति की जाएगी तब यह नई संभावना जन्म लेगी कि किस प्रकार मनुष्य अपने दिल से भगवान् की ओर जा सकता है, किस प्रकार व्यक्ति सारे विधानों से और सारे साधनों के नियमों से ऊपर उठकर सीधे और शक्तिशाली तरीके से आगे जा सकता है, और तभी उन्हें सच्ची संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। और इसके आगे फिर श्रीराधा शक्ति का निरूपण होना तो मनुष्यजाति की आत्मा के लिए बहुत शक्तिशाली चीजें प्रकट करना था। मनुष्य के अन्दर परमात्मा की अनन्त भवितव्यताएँ हैं। और समय-समय पर अवतार इन भवितव्यताओं को उद्घाटित करने के लिए तथा आगे का मार्ग दिखाने के लिए आते रहते हैं। अवतार को हम इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और उनके काम को पूरा करने के लिए जितने ज्ञान और शक्ति की उन्हें आवश्यकता है वे उतनी ही शक्ति-सामर्थ्य धारण करते हैं, उससे कम या अधिक नहीं। भगवान् को अपनी शक्ति-सामर्थ्य का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना होता। सर्वशक्तिमान् होते हुए भी उन्हें मनुष्य को ऐसा दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम समझ सकें तो, अपने-आप को सीमित कर लेना उनकी सर्वशक्तिमत्ता का ही सूचक है। जब भगवान् स्वयं अचेतन जड़तत्त्व बन जाते हैं तो यह उनकी महत्तम भगवत्ता की निशानी है। वस्तुतः जो सर्वज्ञ है वही मूढ़ बन सकता है। ये सभी सीमितताएँ भगवान् की सर्वशक्तिमत्ता को कुछ कम नहीं करतीं अपितु उनकी महत्तम शक्तिमत्ता की प्रत्यक्ष सूचक हैं।
इस प्रकार मानवजाति की अंतरात्मा में सद्गुरुओं, महात्माओं और संतों के द्वारा भगवान् के नए-नए रूप प्रकट होते रहते हैं और नई-नई चीजें आती रहती हैं। परन्तु वे भी एक निश्चित सीमा में बँधे रहते हैं। पर भगवान् का व्यक्तित्व जब स्वयं प्रकट होता है तो एक बहुत बड़ा उत्थान होता है, एक नया दृष्टिकोण सामने आता है, जो पहले कभी नहीं था। जैसे, श्रीचैतन्य महाप्रभु अपने प्राकट्य के साथ एक नवीन चीज लाए। हालाँकि उनके आविर्भाव से पूर्व भी वैष्णव थे, और भगवान् के प्रति भक्ति भी थी परन्तु श्रीचैतन्य महाप्रभु जिस तरीके से संकीर्तन को उजागर किया और भगवान् के प्रति प्रेम की जैसी पराकाष्ठा को अभिव्यक्त किया और उसकी जैसी अभिव्यक्ति उनके जीवन में हुई वह बहुत विलक्षण चीज थी और इससे एक नई चीज जुड़ी जो पहले कभी नहीं हुई थी। वैसे ही, जब श्रीमाँ व श्रीअरविन्द आए तो उन्होंने चेतना के विकास में एक नई चीज को जोड़ा। इस प्रकार यही हमारे लिए अवतार की सबसे बड़ी व्यावहारिक बात है। अवतारों को कोई अपने चमत्कार या जादूगरी दिखाने की कोई बाध्यता नहीं होती, उन्हें जो उपयुक्त लगता है वह होता है और बाकी किसी चीज की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वे उन दुष्टों का विनाश न करें जो भागवत् कार्य में बाधा खड़ी कर रहे हों। उनका विनाश तो श्रीराम ने भी किया और श्रीकृष्ण ने भी किया। परन्तु यह भी कोई आवश्यक चीज नहीं है। आवश्यक तो है मनुष्यजाति की चेतना में जो संकटावस्था उपस्थित हो जाती है उसे हल करना। यदि वह हल उसे कोई नया प्रकाश दिखाने से, कोई नया आयाम जोड़ने से होता हो तो वैसा किया जाएगा और यदि उसमें कोई भौतिक बाधाएँ या संकट उपस्थित हों तो उन्हें दूर कर के किया जाएगा।
वर्तमान समय में जो संकटावस्था उपस्थित है उसमें भगवान् की अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक है क्योंकि यह अवस्था केवल मानसिक विचारों से टूटने वाली नहीं है। इसके लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जिसके सामने मिथ्यात्व आदि सभी चीजें त्रस्त, ध्वस्त हो जाएँ। इसके लिए आवश्यक है कि एक नया अंतःप्रकाश, एक नया अंतःप्रकटन आए जो वर्तमान समस्याओं को विजयी रूप से संभाल सके। आज विज्ञान, तकनीकी आदि क्षेत्रों में मनुष्य ने बहुत अधिक वृद्धि कर ली है जबकि उसका उपयोग करने वाली चेतना में कोई सच्ची वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए इन सभी शक्तिशाली साधनों को उसकी स्वार्थमय और अहमात्मक चेतना ही उपयोग में लेती है और इससे मनुष्यजाति के सामने एक बड़ा भारी संकट पैदा हो गया है। इसलिये एक ऐसी चेतना की आवश्यकता है जो इन सभी चीजों को अपने उचित स्थान में रख सके और इनके साथ यथोचित व्यवहार कर सके।
वर्तमान समय में तो मनुष्यजाति विज्ञान की तरक्कियों से चकाचौंध हो रही है। ऐसे में जिन लोगों में कुछ आंतरिक समझ है, उनके लिए भी यह देख पाना कठिन हो गया है कि आखिर आध्यात्मिकता और विज्ञान का भविष्य में क्या समीकरण होगा। इसलिए आवश्यकता है कि भगवान् का एक ऐसा व्यक्तित्व प्रकट हो जो इन सभी चीजों को समन्वित करने और मनुष्यजाति के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करने की सामर्थ्य रखता हो। श्रीमाँ व श्रीअरविन्द मोटे रूप में तो सारा प्रारूप हमें दे ही चुके हैं। यदि वे ही पुनः आकर इन सारी बाधाओं को दूर कर मार्ग प्रशस्त करते हैं तो यह कोई अनहोनी बात नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए। यदि वे प्रकट होकर यह काम करें तभी चेतना की इस संकटावस्था से मनुष्यजाति निकल सकती है अन्यथा दिव्य जीवन के संदेश को मनुष्यजाति के लिए आत्मसात् करना आसान नहीं है। श्रीकृष्ण-भक्ति के संदेश को श्रीचैतन्य महाप्रभु ने ही शक्तिशाली रूप से अभिव्यक्त किया। इसलिए क्यों ऐसा संभव नहीं है कि श्रीअरविन्द व श्रीमाँ ही अपने कार्य की पूर्णाहुति के लिए पुनः स्वयं ही आ जाएँ। क्योंकि यह काम परमात्मा स्वयं ही कर सकते हैं, अन्य किसी में इसे करने का सामर्थ्य नहीं है।
अवतार एक महान् आध्यात्मिक गुरु या परित्राता के रूप में, बुद्ध और ईसा के रूप में अवतरित हो सकते हैं किन्तु उनकी पार्थिव अभिव्यक्ति की समाप्ति के बाद सदा ही उनके कर्म के फलस्वरूप जाति के केवल नैतिक जीवन में ही नहीं अपितु उसके सामाजिक और बाह्य जीवन और आदशों में भी एक गंभीर और शक्तिशाली परिवर्तन आता है। दूसरी ओर, वे दिव्य जीवन, दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य शक्ति की विशिष्ट क्रिया के अवतार के रूप में, किसी ऐसे कार्य या मिशन के लिए अवतरित हो सकते हैं जो बाह्य रूप से सामाजिक, नैतिक और राजनैतिक दिखायी देता हो; जैसा कि राम और कृष्ण की कथाओं में दर्शाया गया है; परंतु सदा ही यह अवतरण जाति की आत्मा में उसके आंतरिक जीवन के लिए और उसके आध्यात्मिक नवजन्म के लिए एक स्थायी शक्ति का काम करता है। सचमुच ही यह एक अनोखी बात है कि बौद्ध और ईसाई धर्मों का स्थायी, जीवंत तथा व्यापक फल यह हुआ कि जिन मनुष्यों तथा कालों ने इनके धार्मिक और आध्यात्मिक मतों, रूपों और साधनाओं का परित्याग कर दिया, उन पर भी इन धर्मों के नैतिक, सामाजिक और व्यावहारिक आदर्शों का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा।... वहीं दूसरी ओर, राम और कृष्ण की जीवनलीला ऐतिहासिक काल के पूर्व की है, जो काव्य और कथा के रूप में हमें प्राप्त हुई है और इसे हम केवल काल्पनिक कहानी भी कह सकते हैं; परंतु इन्हें हम काल्पनिक कहानी मानें या ऐतिहासिक तथ्य, यह सर्वथा महत्त्वहीन है; क्योंकि उनका शाश्वत सत्य और महत्त्व तो जाति की आंतरिक चेतना और मानव-आत्मा के जीवन में सतत् एक आध्यात्मिक रूप, उपस्थिति और प्रभाव के रूप में बने रहने में निहित है। अवतार दिव्य जीवन और चेतना का एक तथ्य हैं जो अपने-आप को किसी बाह्य कर्म में भी चरितार्थ कर सकते हैं, परंतु जो अवश्य ही उस कर्म के संपन्न हो जाने के बाद भी एक आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में बने रहते हैं; अथवा वे अपने-आप को किसी आध्यात्मिक प्रभाव या शिक्षा में संसिद्ध या चरितार्थ कर सकते हैं, किन्तु उस नये धर्म या साधना के क्षीण हो जाने पर भी, मानवजाति के विचार, उसकी मनोवृत्ति और उसके बाह्य जीवन पर उनका स्थायी प्रभाव अवश्य बना रहता है।
यहाँ श्रीअरविन्द ने बुद्ध का, ईसा का, श्रीराम का और श्रीकृष्ण का उदाहरण दिया है। हमने पहले भी यह चर्चा की थी कि अवतार के पार्थिव जगत् से चले जाने के बाद भी उनका प्रभाव बना रहता है। उनकी उपस्थिति सूक्ष्म जगत् में बनी रहती है और वे जिसमें भी ग्रहणशीलता पाते हैं वहीं उनके लिये संकल्प और सहायता करते रहते हैं। इसीलिये न तो श्रीराम का कार्य और प्रभाव रुका है और न श्रीकृष्ण का। ये अवतार ऐतिहासिक थे या नहीं थे उससे फर्क नहीं पड़ता। महत्त्व इस बात का है कि वे आज भी मौजूद हैं और सक्रिय हैं। हम उनसे आज भी सम्पर्क कर सकते हैं। उनके अस्तित्व के निश्चित प्रमाण भी मिल रहे हैं पर ये सभी कथाएँ ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के आधार पर रूपक के रूप में निर्मित की गई हैं। परन्तु अभी वह चर्चा का विषय नहीं है। मुख्य बात है कि अवतारों का प्रभाव सदा बना रहता है।
दूसरी बात यह है कि, हमारे सामने एक उदाहरण गौतम बुद्ध, ईसा मसीह का है। इनका जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक था। इनका सामाजिक, राजनैतिक अथवा आर्थिक जीवन से कोई संबंध नहीं था। इनका संदेश आध्यात्मिक था। उसे हम चाहे धार्मिक अथवा नैतिक कोई भी नाम दे दें। परन्तु जिन व्यक्तियों ने इनके आध्यात्मिक अथवा धार्मिक संदेश को चाहे माना या नहीं माना, उनके भी सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक जीवन पर इन अवतारों का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। इनका प्रभाव केवल आध्यात्मिक पक्ष तक ही सीमित नहीं था। इनका मनुष्यजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और बाहरी जीवन पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा है, जिन व्यक्तियों ने इनको माना उन पर भी और जिन्होंने नहीं माना उन पर भी। केवल एक आत्मा के उत्थान में ही नहीं अपितु साथ-ही-साथ समष्टि में भी कोई नयी चीज भगवान् के व्यक्तित्व के कारण ही आती है। दूसरी तरफ श्रीराम और श्रीकृष्ण का उदाहरण है। इनके जीवन को यदि हम देखें तो लगता है कि इन्हें पारंपरिक आध्यात्मिकता, योग-साधना आदि से तो कोई विशेष सरोकार ही नहीं था। श्रीकृष्ण के जीवन को तो हम गीता में उनके संदेश के कारण आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं परन्तु श्रीराम के जीवन से तो अधिक ऐसा प्रकट नहीं होता कि प्रचलित आध्यात्मिकता से उनका विशेष कोई संबंध रहा हो। वह तो प्रकट रूप से पूर्णतः नैतिक, राजनैतिक व्यवस्था, समाज की व्यवस्था से संबंधित दिखता है। भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म भी असुरों और अनाचार के नाश के लिए ही हुआ था। परंतु उनका प्रभाव जाति के बाह्य जीवन में ही धर्म की स्थापना के लिए उतना नहीं होता जितना कि आध्यात्मिक मार्ग खोलने के लिए होता है। श्रीराम से, श्रीकृष्ण से जुड़ कर कितने ही लोग अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। उनका जीवन के सामाजिक, आर्थिक आदि पहलुओं पर उतना प्रभाव नहीं है जितना कि आध्यात्मिकता पर है, जो कि प्रत्यक्षतः उन्होंने नहीं की। अतः अवतार अपनी लौकिक अभिव्यक्ति में क्या करता है उसी से वह सीमित नहीं होता। उसके व्यक्तित्व में जो चीजें हैं वे हमें बाद में भी मिलती रहती हैं। आज श्रीकृष्ण प्रधान रूप से अध्यात्म की ओर ले जाने वाले व्यक्तित्व हैं। श्रीराम जी भी उसी ओर ले जाने वाले व्यक्तित्व हैं। आज उनका प्रभाव प्रत्यक्षतः सामाजिक व्यवस्था आदि पर उतना न होकर अध्यात्म पर अधिक है। और यह बड़ी विलक्षण बात है। अर्थात् अवतार अपने जीवन में क्या अभिव्यक्त करते हैं और क्या नहीं, उससे अधिक फर्क नहीं पड़ता। परंतु मुख्य बात तो उनके पीछे जो तत्त्व विद्यमान है उसकी है। इसीलिए श्रीमाँ व श्रीअरविन्द ने अपनी शिक्षा में जो कुछ भी बताया है उनका प्रभाव और प्रकाश उतने भर तक ही सीमित नहीं है, वह तो उनके पूर्ण प्रकाश का एक क्षुद्र अंश ही है, और उसके पीछे और भी अनंत संभावनाएँ निहित हैं। इसलिए श्रीमाँ व श्रीअरविन्द का जो अपना सच्चा स्वरूप था वह भी विद्यमान है और वह भी मनुष्यजाति में उँड़ेला जा रहा है। उसका प्रभाव यथासमय प्रकट होगा, उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी क्रिया अमोघ है और उसका प्रभाव अवश्य होगा क्योंकि यह वस्तुओं की गति में अवश्यंभावी है। श्रीकृष्ण के जाने के कितने वर्षों बाद में ये चीजें आरम्भ हुई। उसकी तुलना में अब तो प्रक्रिया बड़ी ही तीव्र गति से चल रही है। हम यह कह सकते हैं कि श्रीमाँ व श्रीअरविन्द ने यहाँ जो कुछ प्रत्यक्षतः किया, जो कुछ संभावनाएँ वे लेकर आए, या जो कुछ उन्होंने बताया वह तो उनको वास्तविकता का बहुत थोड़ा-सा ही अंश है। श्रीकृष्ण के जीवन को ही लें तो हम कहेंगे कि उनके बाहरी जीवन में तो वैसी कोई बातें थी ही नहीं जिस प्रकार के तत्त्व का भागवत् में निरूपण हुआ है। वैसे ही श्रीमाँ व श्रीअरविन्द जो चीजें लाए उनमें से कुछ तो अभिव्यक्त हुई हैं परन्तु शेष सारी तो अभिव्यक्त होनी अभी बाकी हैं, जो कि निश्चित रूप से अभिव्यक्त होंगी ही। उनकी उपस्थिति पार्थिव वातावरण को छोड़ने वाली नहीं है। श्रीमाताजी ने साफ-साफ ही यह कहा है कि श्रीअरविन्द धरती को छोड़ कर दूर नहीं जाएँगे जब तक कि अतिमानसिक रूपांतरण का उनका कार्य संपन्न नहीं हो जाता। इसलिये हमें किसी भी तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भाग में हमारे लिए यह बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि हम इस बात पर सच्चे रूप में विश्वास न कर के सतही चीजों से और भौतिक विज्ञान आदि की बाहरी प्रतीतियों की चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए इस अवतार तत्त्व को लेकर यदि हम इसे वर्तमान पर लागू कर के इसे न समझें तो केवल अतीत की ही बातें करने से कोई लाभ नहीं है। उनकी उपस्थिति हमारा मार्गदर्शन करेगी और यह काम किये बिना छोड़ेगी नहीं। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम निश्चिंत होकर सो जाएँ, और अपना प्रयास करना बंद कर दें। हमारी भावना होनी चाहिये कि हम उनके कार्य में सहयोग करें। भले ही उसका अपने-आप में कितना भी महत्त्व हो या न हो। परंतु कम-से-कम उन ग्वाल बालों की तरह हम अपना प्रयास तो कर ही सकते हैं जिन्हें यह भ्रम था कि गोवर्धन को उन्होंने अपनी लाठियों के सहारे रोके रखा है। इतना तो हम अवश्य ही कर सकते हैं।
इसलिए अवतार के कार्य के विषय में गीता के वर्णन को ठीक तरह से समझने के लिए हमें धर्म शब्द को अवश्य ही इसके परिपूर्णतम, गंभीरतम और विस्तृततम अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, उस आंतर और बाह्य विधान के रूप में समझना चाहिए जिसके द्वारा दिव्य संकल्प और प्रज्ञा मानवजाति के आध्यात्मिक विकास को साधने का काम करते और जाति के जीवन में उसकी विशिष्ट परिस्थितियों और उनके परिणामों को निर्मित करते हैं।
गीता उस संघर्ष पर बल देती है जिसका कि यह जगत् रंगमंच है, अपने दो पहलुओं में यह है एक आंतरिक संघर्ष और दूसरा बाह्य युद्ध। आंतरिक संघर्ष में शत्रु अन्दर, व्यक्ति के अपने अन्दर हैं, और इसमें कामना, अज्ञान और अहंकार को मारना ही विजय है। परंतु मानव-समष्टि के अन्दर धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच एक बाह्य युद्ध भी चल रहा है.... इस बाह्य संग्राम में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने, असुरों अर्थात् दुष्टों के राज्य को नष्ट करने, वे जिस (आसुरी) शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका दमन करने और उनके द्वारा उत्पीड़ित धर्म के आदर्शों को पुनः स्थापित करने के लिए अवतार आते हैं। वे व्यष्टिगत मानव-आत्मा के अंदर स्वर्गराज्य का निर्माण करने के लिए आते हैं और साथ ही मानव-समष्टि के लिए भी स्वर्गराज्य को पृथ्वी के निकटतर ले आने के लिए आते हैं।
यहाँ यह स्पष्ट ही है कि अवतार धरती पर धर्म की स्थापना के लिये आते हैं। पर अपने विस्तीर्णतम अर्थ में धर्म का अभिप्राय है व्यष्टि और समष्टि को भागवत् संकल्प एवं भागवत् ज्ञान द्वारा भागवत् पथ पर निर्देशित करना। और इस धर्म की रक्षा करने तथा इसे और अधिक समृद्ध बनाने के लिये भगवान् अवतार लेते हैं। अवतार इसी की तैयारी कराते हैं और इस उद्देश्य में बाधक सभी बाहरी बाधाओं को, सभी आसुरिक ताकतों को, जो समष्टिगत जीवन को नियंत्रण में रखना और पथ पर बढ़ने से रोकना और भ्रमित करना चाहती हैं, नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार अवतार-संबंध में सारी बातों का स्पष्टीकरण हो गया कि वे किस उद्देश्य से आते हैं, धरती पर उनका क्या-क्या प्रभाव होता है और उनके बाद भी किस प्रकार उनकी उपस्थिति सूक्ष्म रूप से सदा ही बनी रहती है। इसके अतिरिक्त अवतार तत्त्व से संबंधित अन्य अनेक पहलुओं की हम चर्चा कर चुके हैं।
श्रीअरविन्द के अनुसार अवतार को जो विशिष्ट कार्य करना होता है उसकी वे अपने पूर्व के जन्मों में तैयारी करते हैं। गीता में भी भगवान् कृष्ण कह रहे हैं कि उनके इस जन्म से पूर्व भी अनेकों जन्म हो चुके हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी अवतारी जन्म ही हों। उसी प्रकार श्रीमाताजी व श्रीअरविन्द भी सदा ही मौजूद रहे हैं, परन्तु अवतार के रूप में नहीं। और पूर्वजन्मों में उनके उस तत्त्व की तैयारी चलती रहती है जिसकी उन्होंने अवतार के रूप में जन्म ग्रहण कर के अभिव्यक्ति की। इसलिए भगवान् का जन्म कोई आकस्मिक प्रकटन ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। उसके पीछे हजारों वर्षों की तैयारी हो सकती है जिससे कि जो संदेश उन्हें देना है वह मनुष्यजाति द्वारा ग्रहण किया जा सके। और इस दौरान मनुष्यजाति की भी तैयारी होती है कि उस तत्त्व को वह ग्रहण कर सके। तभी तो गीता में भगवान् कहते हैं कि 'जन्म कर्म च मे दिव्यं' और जो इसको तत्त्वतः जान लेता है वह पुनः जन्मबंधन में नहीं पड़ता। यह बहुत ही गहरी बात है जिसे समझना आसान नहीं है। श्रीअरविन्द इतना कुछ इस विषय में बता गए हैं तभी हमें इसके विषय में कुछ प्रकाश प्राप्त होता है अन्यथा तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसे समझने के लिए व्यक्ति को स्वयं इसका व्यक्तिगत अनुभव होना आवश्यक है अन्यथा इसे समझने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और चूंकि श्रीअरविन्द को इसका निजी अनुभव था और साथ ही उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता भी अद्वितीय थी, इसलिए हमारे लिए इस तत्त्व के संबंध में कुछ समझ पाना सुगम हो गया है।
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।। १० ।।
१०. राग, भय और क्रोध से मुक्त, अपनी चेतना (चित्त) के भीतर मुझ से परिपूर्ण हुए अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ मेरा आश्रय ग्रहण किये हुए बहुत से मनुष्य ज्ञानरूपी तप से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हो गये हैं।
अवतार के आने का आंतरिक फल उन लोगों द्वारा लाभ किया जाता है जो इस क्रिया से दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के वास्तविक मर्म को जान लेते हैं, और जो अपनी चेतना में भगवान् से परिपूर्ण होकर, अपनी संपूर्ण सत्ता सहित उनमें आश्रित होकर (मन्मया मामुपाश्रिताः) रहते हैं और अपने ज्ञान की तपःशक्ति से पवित्र होकर (ज्ञानतपसा पूताः) निम्न (अपरा) प्रकृति से मुक्त होकर भगवान् के स्वरूप और स्वभाव (मद्भावम्) को प्राप्त होते हैं। मनुष्य के अन्दर इस अपरा प्रकृति के ऊपर जो दिव्य प्रकृति है उसे प्रकटाने के लिए तथा यह दिखाने के लिए कि मुक्त, निरहंकार, निष्काम, नैयक्तिक, विश्वव्यापक, दिव्य-ज्योति, दिव्य-शक्ति और दिव्य-प्रेम से परिपूर्ण दिव्य कर्म क्या होते हैं, अवतार का आगमन होता है। वे उस दिव्य व्यक्तित्व के रूप में आते हैं जो मनुष्य की चेतना को परिपूर्ण कर देगा और उसके अहंभावापत्र परिसीमित व्यक्तित्व की जगह ले लेगा जिससे कि वह अहंकार से मुक्त होकर अनन्तता और विश्वव्यापकता में फैल जाए, जन्म (बंधन) से मुक्त होकर अमरत्व में पहुँच जाए। भगवान् उस दिव्य शक्ति और प्रेम के रूप में आते हैं, जो मनुष्यों को अपनी ओर बुलाते हैं ताकि मनुष्य उन्हीं का आश्रय लें तथा अब और अधिक अपने मानवसंकल्पों की अपर्याप्तता का तथा अपने काम-क्रोध और भय के द्वन्द्वों का आश्रय न लें, और इस सब अशांति और दुःख से मुक्त होकर भगवान् की शान्ति और आनन्द में निवास करें।
अवतार के जीवन से, उसकी घटनाओं से, उसकी दिव्य कथाओं से, लीलाओं से परिपूर्ण होकर जो ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रयोग में लाकर उससे पवित्र होकर (मद्भावम् आगताः) भगवान् के स्वभाव और स्वरूप को प्राप्त होना होता है। सबसे पहले व्यक्ति अपने सतही भाव में रहता है, उससे आरोहण कर के उसे अपने स्वभाव की ओर जाना होता है और फिर उस स्वभाव से 'मद्भाव' अर्थात् भगवान् के भाव को प्राप्त करना होता है। अवतार इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे श्रीमाँ व श्रीअरविन्द के आने से कितने ही लोग भगवान् के मार्ग पर चल पड़े जबकि अपने-आप से कदाचित् ही वे कभी इस पथ को अपनाते या इस पर अधिक दूरी तक जा पाते। क्योंकि जब तक मनुष्य के हृदय का भगवान् से जीवंत संपर्क न हो तब तक केवल बुद्धि और सीमित इच्छा-शक्ति के बल पर व्यक्तिगत गठन को और इसके चक्करों को, इसी के अंदर व्यक्ति की तल्लीनता को तोड़ पाना बहुत कठिन है। और यदि कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य से कुछ ग्रहण कर भी लेता है तो वह आंशिक प्रकाश होता है, पूरा प्रकाश उसके जीवन में मुश्किल से ही आता है। और अधिकांश लोगों के जीवन में तो प्रकाश की वह किरण भी नहीं आती। इसलिए भगवान् की सशरीर उपस्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है। उनकी वह सशरीर उपस्थिति तिरोहित होने के बाद भी बहुत से लोग उस ओर प्रेरित होते हैं, जिससे उनके जीवन में भगवान् का बहुत बड़ा प्रवेश होता है।
-----------
* एक पारस्परिक ऋण मानव को परम् से बाँधता हैः
उसकी प्रकृति को हमें वैसे ही धारण करना होगा जैसे उसने हमारी धारण की है;
हम भगवान् के पुत्र हैं और अवश्य ही उनके सदृश होना होगाः
उसके मानवीय अंश, हमें दिव्य बनना है।
हमारा जीवन एक पहेली है जिसकी कुंजी है भगवान्।
जिन लोगों को कभी श्रीमाँ व श्रीअरविन्द का भौतिक सम्पर्क नहीं मिला वे भी उनकी सूक्ष्म उपस्थिति के कारण इस ओर मुड़ जाते हैं और उनके जीवन में भी उनका प्रकाश प्रवेश कर जाता है क्योंकि वे सूक्ष्म वातावरण में सारी आवश्यक सामग्री छोड़ कर गये होते हैं जिसे हम आत्मसात् कर सकते हैं। अतः भगवान् का अवतार लेना एक बहुत ही विशिष्ट क्रिया है जिसमें भगवान् के व्यक्तित्व के नए-नए आयाम प्रकट होते हैं। अन्यथा व्यक्ति जिस साधारण चेतना में निवास करता है उससे परम् चेतना की ओर जाना संभव ही नहीं होता। यह सब दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान की व्यवस्था है कि किस प्रकार मनुष्यजाति में भगवान् का पूर्ण प्राकट्य सिद्ध हो। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सन्त, महापुरुष, देवता और अवतार आदि आते रहते हैं ताकि यह क्रम निर्बाध और अटूट रूप से चलता रहे। यह अवतार के आने का मूलभूत उद्देश्य है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर दिव्य जीवन का कार्य संपन्न न हो। हिन्दुस्तान तो विशेषकर परमात्मा की एक चुनी हुई भूमि है, उनका कार्यक्षेत्र है। इसलिए यहाँ तो यह कार्य होना ही है।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।। ११ ।।
११. हे पार्थ ! मनुष्य जिस किसी भी रूप से मेरे समीप आते हैं उन्हें मैं उस ही रूप में प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हूँ, मनुष्य हर प्रकार से मेरे द्वारा निर्धारित किये हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं।
यह बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है कि हम भगवान् से जैसी आशा करते हैं वे वैसे ही बन जाते हैं। जिस रूप में हम उनकी चाह करते हैं वे उसी रूप को धारण कर लेते हैं क्योंकि उनके अनन्त रूप हैं पर अपने किसी भी रूप से वे सीमित नहीं हैं। सारे रूप उन्हीं के हैं पर फिर भी कोई भी रूप उनका नहीं है। जैसे-जैसे मनुष्य की चेतना विकसित होती है वैसे-वैसे उसके लिए उनका रूप भी बदलता जाता है। पशु की चेतना के लिए मनुष्य ही भगवान् हैं, वैसे ही शुरू में मनुष्यों के लिए देवता भगवान् की तरह होते हैं। और ज्यों-ज्यों मनुष्य की चेतना विकसित होगी त्यों-त्यों उसके सामने भगवान् का और अधिक विशाल रूप प्रकट होता जाएगा। सारे रूप भगवान् के ही हैं परन्तु मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें महसूस करता है। तभी तो भगवान् कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। सभी लोग सभी तरीके से मेरे ही मार्ग पर चल रहे हैं। 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः'। इसी की पुष्टि करते हुए श्रीमाताजी ने यहाँ अपना निजी अनुभव भी बता दिया।
------------------------------
* भगवान् हर एक व्यक्ति को ठीक वही देते हैं जिसकी वह उनसे आशा करता है। यदि तुम यह मानते हो कि भगवान् बहुत दूर और क्रूर हैं, तो वे दूर और क्रूर होंगे, क्योंकि ऐसा तुम्हारे परम कल्याण के लिये आवश्यक होगा कि तुम भगवान् के कोप का अनुभव करो; काली के उपासकों के लिये वे काली होंगे और भक्त के लिये 'परमानन्द'। और वे ज्ञान के जिज्ञासु के 'सर्वज्ञान' होंगे, मायावादियों के परात्पर 'निर्गुण ब्रह्म'; नास्तिक के साथ वे नास्तिक होंगे और प्रेमी के प्रेम... वस्तुतः भगवान् वही हैं जिसकी तुम उनसे अपनी गहरी-से-गहरी अभीप्सा में आशा करते हो।
और जब तुम उस चेतना में प्रवेश करते हो जहाँ तुम सभी चीजों को एक ही दृष्टि में देखते हो, मनुष्य और भगवान् के बीच संबन्धों की अनंत बहुलता को देखते हो, तो तुम देखते हो कि अपने सभी ब्यौरों सहित यह कैसा अद्भुत है। तुम मनुष्यजाति के इतिहास पर दृष्टिपात कर सकते हो और यह देख सकते हो कि मनुष्य जो समझे हैं, उन्होंने जिसकी इच्छा और आशा की है, जिसके स्वप्न देखे हैं, उसके अनुसार भगवान् कितने विकसित हुए हैं। और किस प्रकार वे जड़वादी के साथ जड़वादी रहे हैं और किस प्रकार वे प्रतिदिन विकसित होते जाते हैं और जैसे-जैसे मानव चेतना अपने-आपको विस्तृत करती जाती है वैसे ही वे भी दिन-प्रतिदिन निकटतर तथा और अधिक प्रकाशमान होते जाते हैं....
भगवान् तुम्हारी अभीप्सा के अनुसार तुम्हारे साथ हैं। स्वभावतः इसका यह अर्थ नहीं है कि वे तुम्हारी बाह्य प्रकृति की सनकों के आगे झुक जाते हैं, - यहाँ मैं तुम्हारी सत्ता के सत्य की बात कह रही हूँ। और फिर भी, कभी-कभी भगवान् अपने-आपको तुम्हारी बाह्य अभीप्साओं के अनुसार भी गढ़ते हैं... इस प्रकार मनोभाव, यहाँ तक कि बाहरी मनोवृत्ति भी, बहुत महत्त्वपूर्ण है। लोग नहीं जानते कि श्रद्धा कितनी महत्त्वपूर्ण है, किस प्रकार श्रद्धा चमत्कार है, चमत्कारों की सर्जक है। यदि तुम प्रतिक्षण ऊपर उठाए जाने और भगवान् की ओर खींचे जाने की आशा करो, तो वे तुम्हें उठाने आएँगे और वे वहाँ उपस्थित होंगे, बहुत निकट, निकटतर, अधिकाधिक निकट होंगे।
प्रश्न : 'कभी-कभी भगवान् अपने-आप को तुम्हारी बाह्य अभीप्साओं के अनुसार भी गढ़ते हैं... इस प्रकार मनोभाव, यहाँ तक कि बाहरी मनोवृत्ति भी, बहुत महत्त्वपूर्ण है।' इसका क्या तात्पर्य है?
उत्तर : एक स्त्री ने श्रीमाताजी से पूछा कि मैं तो भगवान् के लिए ही सब काम करना चाहती हूँ। परन्तु इसमें एक समस्या यह आती है कि जब मैं चाय बनाती हूँ तो मुझे यह कैसे पता चले कि उनको चीनी कितनी पसन्द है। इसके उत्तर में श्रीमाताजी ने कहा कि भगवान् के यहाँ इन चीजों का कोई महत्त्व नहीं है, महत्त्व तो केवल उस भाव का है जिससे वह कार्य किया जाता है। परन्तु बाद में इसी संदर्भ में श्रीमाँ ने संशोधन करते हुए कहा कि भगवान् को चाय में कितनी चीनी पसंद है यह जानना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उनका अपना स्वाद होता है। और यदि हम उनसे सही रूप से पूछेंगे तो वे अवश्य ही बता देंगे कि उन्हें कौनसी चीज कितनी मात्रा में पसंद है। हमें जो और जितना जानना आवश्यक होता है उतना सहज रूप से ही वे हमें अवश्य बता देते हैं। हालाँकि सभी के लिए उनके मापदण्ड एक समान नहीं होंगे परंतु व्यक्ति-विशेष के लिए उनका विशिष्ट मापदण्ड होगा। और वास्तव में वे क्या चाहते हैं वह उसे अवश्य ही बता देते हैं। यह बड़ी विचित्र चीज है। इसमें श्रीमाताजी ने एक और सूत्र बताया कि जैसे, व्यक्ति के मन में बड़ी इच्छा होती है कि वह भगवान् के अनुसार काम करे, मन शुद्ध हो, कोई गलत काम नहीं हो परन्तु अपनी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने के लिए उससे गलत काम तो चौबीसों घंटे होते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए। तब श्रीमाताजी ने कहा कि इसका तो एक ही तरीका है कि जैसे ही हमें याद आये कि हम गलती पर हैं उसी क्षण उनसे (श्रीमाँ) से प्रार्थना करनी चाहिए कि 'मेरी इच्छाएँ और कामनाएँ मेरे वश में नहीं हैं इसलिए आप मुझे इनसे छुटकारा दिलाएँ।' तो श्रीमाताजी हमारे अन्दर से इन चीजों को समाप्त करना आरम्भ कर देंगी। यह तरीका तो बहुत अच्छा है कि केवल श्रीमाताजी को बोलने भर से ही काम हो जाएगा। इसमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। श्रीअरविन्द ने कहा कि मैं अपने निजी सामर्थ्य की बजाय भागवत् शक्ति से ही कार्य साधित करवाना पसन्द करता हूँ। यह तो बड़ा ही कारगर सूत्र है। परन्तु हम लोग अहं से इतने भरे रहते हैं कि न हमें यह याद ही रहता और न ही यह सोच ही सकते हैं कि भगवान् को कहें कि ये सब चीजें ठीक नहीं हैं। परन्तु यदि व्यक्ति भगवान् को उस समस्या के विषय में बोलता है तो उसी समय वह भागवत् शक्ति की ओर खुल जाता है और भगवान् की शक्ति उसके अन्दर कार्य करने लगती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि धीरे-धीरे निम्न प्रकृति की ये चीजें बदलती चली जाएँगी, परिस्थितियाँ बदलती जाएँगी और हम उनसे ऊपर उठ जाएँगे। इसलिए व्यावहारिक तरीका है कि कोई समस्या हो तो श्रीमाताजी को बोल दो और विश्वास रखो कि यदि माँग उचित होगी तो वह निश्चित रूप से पूरी होगी। श्रीमाताजी से कुछ माँगने से हम उनके प्रति खुल जाते हैं। इस दृष्टिकोण की बजाय कि 'मैं श्रीमाँ से क्या माँगू क्योंकि मैं तो स्वार्थी नहीं होना चाहता', जबकि वास्तव में तो हम स्वार्थ से तो पूरी तरह भरे रहते हैं, अच्छा हो कि श्रीमाँ से आदान-प्रदान का एक संबंध स्थापित हो जाए तो सारा जीवन ही बदल जाता है।
प्रश्न : यदि तुम यह मानते हो कि भगवान् बहुत दूर और क्रूर हैं, तो वे दूर और क्रूर होंगे, क्योंकि ऐसा तुम्हारे परम कल्याण के लिये आवश्यक होगा कि तुम भगवान् के कोप का अनुभव करो;" फिर आगे कहा है कि "भगवान् तुम्हारी अभीप्सा के अनुसार तुम्हारे साथ हैं। स्वभावतः इसका यह अर्थ नहीं है कि वे तुम्हारी बाह्य प्रकृति की सनकों के आगे झुक जाते हैं," तो फिर इन दोनों बातों में समन्वय कैसे होगा?
उत्तर : यदि हम उनको दूर और क्रूर मानेंगे तो हम अपनी किसी भी आवश्यकता की उनसे माँग ही नहीं करेंगे। वह तो असंगत बात होगी। जो व्यक्ति अपनी बाहरी प्रकृति के अनुसार भगवान् से कुछ करवाना चाहता है इसका अर्थ है कि पहले ही वह बहुत कुछ भगवान् के प्रति खुल चुका है। अन्यथा हमारी बाहरी प्रकृति में तो भगवान् पर विश्वास होता ही नहीं है। लोग प्रार्थना करते हुए भी भीतर से यह जानते हैं कि प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा क्योंकि आखिर सभी काम तो स्वयं ही करने होंगे। गीता में आगे आयेगा कि किस प्रकार व्यक्ति भिन्न-भिन्न देवताओं, गंधवों, राक्षसों आदि की पूजा करते हैं और उन्हें उसी के अनुसार फल प्राप्त हो जाते हैं। भगवान् कहते हैं कि यह सब तो केवल इसी लोक से संबद्ध है और बहुत आसान है और इनके परिणाम भी शीघ्र ही मिल जाते हैं। परंतु भगवान् के निकट जाना कठिन है। हालाँकि बाह्य प्रकृति के अनुसार भी भगवान् बहुत बार काम कर जाते हैं। यह बड़ी ही विलक्षण बात है। हमारा सारा तंत्र ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा हुआ है कि किस प्रकार लोग भगवान् के साथ संपर्क में आ जाते हैं। उनके साथ अनेकों प्रकार की लीलाएँ करते हैं, दिन-प्रतिदिन का संबंध स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, श्री कृष्णप्रेम जब भगवान् को भोग लगाते थे तब भगवान् स्वयं आकर उस भोग को ग्रहण करते थे। ऐसी विलक्षण घटनाओं की सत्यता के विषय में पूछे जाने पर श्रीअरविन्द ने कहा कि ऐसी चीजें हो सकती हैं और इस मामले में ऐसा हुआ है। इन सब चीजों से व्यक्ति के जीवन में भगवान् का प्रवेश होता है, परन्तु व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए। कितने-कितने उदाहरण हमें मिलते हैं जिनमें भगवान् अपने भक्तों से किस प्रकार भोग ग्रहण करते हैं, उनकी संकटपूर्ण स्थितियों से उन्हें उबारते हैं, उनके सखा बनकर उनके साथ खेलते हैं और न जाने और कितने ही प्रकार के संबंध स्थापित कर लेते हैं। सारा तंत्र मनुष्य के सभी हिस्सों को भगवान् से जोड़ने का कार्य करता है।
...मनुष्य चाहे जिस किसी तरह भगवान् को अपनाते, उनसे प्रेम करते और उनमें आनन्द लेते हों, भगवान् उन्हें उसी तरह से अपनाते, उनसे प्रेम करते और उनमें आनन्द लेते हैं... क्योंकि मनुष्यों की भिन्न-भिन्न प्रकृति के अनुसार जितने भी विभिन्न मार्ग हैं उन सभी में मनुष्य भगवान् के द्वारा अपने लिए नियत मार्ग पर चल रहे हैं, जो अन्त में उन्हें भगवान् के समीप ले जाएगा। भगवान् का वही पहलू मनुष्यों की प्रकृति के अनुकूल होता है जिसका वे उस समय सबसे अच्छी तरह अनुसरण कर सकते हैं जब भगवान् नेतृत्व करने आएँ...
काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।। १२ ।।
१२. जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में कमाँ के फल की कामना करते हैं वे देवताओं के निहित यज्ञ किया करते हैं, क्योंकि मनुष्यलोक में कर्म से जनित सफलता बहुत शीघ्र और सरलता से प्राप्त हो जाती है।
...अधिकांश मनुष्य... अपने कर्मों की सिद्धि की कामना से, देवताओं के अर्थात् एकमेव परमेश्वर के विविध रूपों और व्यक्तित्वों के प्रीत्यर्थ यज्ञ करते हैं, क्योंकि कर्मों से ज्ञानरहित कर्मों से होनेवाली सिद्धि मानव-जगत् में बहुत शीघ्र और सुगमता से प्राप्त होती है; अवश्य ही वह सिद्धि केवल उसी जगत् की होती है। परन्तु दूसरी सिद्धि, अर्थात् पुरुषोत्तम के प्रीत्यर्थ किये जानेवाले ज्ञानयुक्त यज्ञ के द्वारा मनुष्य की दिव्य आत्मपरिपूर्णता, उसकी अपेक्षा अधिक कठिनता से प्राप्त होती है; इस यज्ञ के फल सत्ता के एक उच्चतर जगत् के होते हैं और कम सुगमता से पकड़ में आते हैं।
यदि व्यक्ति को किसी भी कर्म का फल चाहिए तो - जिस प्रकार का कर्म है, उसे करने के पीछे जैसी भावना है, जिस उद्देश्य से कर्म किया जा रहा है - उसके अनुसार व्यक्ति को उस कर्म के पीछे निहित यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देवता आदि शक्तियों के संपर्क में आना पड़ता है जिनके द्वारा वह कार्य सिद्ध किया जाता है। और जो कर्म उनके साथ आदान-प्रदान से सिद्ध होते हैं उन्हें करना तथा उनके फलों को प्राप्त करना संसार में अपेक्षाकृत सरल होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के मन में आ जाए कि उसे पैसे कमाने हैं तो वह तरह-तरह की चीजों के संपर्क में आता है और अपनी इस कामना की पूर्ति के लिए वह उसमें अपनी एकाग्रता, अपनी मेहनत, अपनी भावना, अपनी इच्छा-शक्ति तथा अपनी संकल्प-शक्ति लगाता है। इस तरीके से व्यक्ति कर्म के पीछे निहित शक्तियों को ये सब चीजें अर्पित करता है तो वे शक्तियाँ भी व्यक्ति को इसका प्रतिफल देती हैं। और यदि व्यक्ति अमुक कर्म को पूर्ण करने का प्रयास करता रहता है तो धीरे-धीरे उसका रास्ता खुलता जाता है। इसी प्रणाली से पूरे विश्व में काम होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति किसी प्रयोजन से कोई कर्म करे पर उसे उसका प्रतिफल न मिले तब तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और संसार में कोई काम ही नहीं होगा। यह तो ईश्वर का ही बनाया हुआ विधान है। इस श्लोक में इसी के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार का लेन-देन, इस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त करना अपेक्षाकृत सरल है, परंतु यह आदान-प्रदान उस प्रतिफल विशेष तक ही सीमित रहता है। और व्यक्ति अपनी इस लेन-देन की क्षमता से कभी ऊपर नहीं उठ सकता। इस स्थिति में जो सफलता मिलती है वह यहीं संसार में रह जाती है और व्यक्ति का अंत समय आने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से व्यक्ति का आन्तरिक विकास बहुत ही कम हो पाता है। कुछ व्यक्ति तामसिक प्रकार के होते हैं। उनकी मानसिकता भी बड़ी ही तामसिक और संकीर्ण होती है। उनके कर्मों के पीछे के हेतु बड़े ही तुच्छ होते हैं, उनका आदान-प्रदान भूतों और पिशाचों से होता है और बहुत श्रम करने पर भी उन्हें बहुत ही कम फल मिल पाता है जैसे कि पशु बहुत श्रम करने पर भी कठिनाई से ही अपना जीवन यापन कर पाता है। यदि व्यक्ति तामसिक मनोस्थिति में है और केवल अपने ही ऊपर केन्द्रित रहता है तो वह बहुत कठिनाई से ही अपना गुजारा कर पाता है। वहीं, यदि कोई दूसरा व्यक्ति तामसिक स्थिति की बजाय कुछ अधिक सुसंस्कृत है, जो अतिशय रूप से केवल अपने ही ऊपर केन्द्रित न रहकर दूसरों के बारे में तथा आपसी तालमेल के बारे में भी सोचता है वह कुछ अधिक श्रेष्ठ शक्तियों के सम्पर्क में होता है और कम मेहनत में ही उसे अधिक फल मिल जाता है। यदि व्यक्ति इससे भी अधिक उच्च स्थिति में हो तो वह और अधिक उच्च शक्तियों के संपर्क में होता है और उसे उसका प्रतिफल और अधिक अच्छा मिल जाता है। इस तरह यह प्रगतिशील है। जैसे पशु को बहुत मेहनत करने पर भी फल की प्राप्ति में अनिश्चितता ही रहती है। उसी प्रकार वह व्यक्ति जिसके अंदर भौंडापन है, बहुत मेहनत करने पर भी उसे बहुत थोड़ा ही प्रतिफल मिल पाता है क्योंकि उसका आदान-प्रदान वैसी ही शक्तियों के साथ होता है। इसी तरीके से संसार चलता है। भगवान् कह रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था है और भूतों, पिशाचों आदि के निमित्त किये कार्यों के परिणाम व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद नहीं करते, वह जहाँ है, उसे वहीं रोके रखते हैं। और जो कर्म भगवान् के निमित्त किये जाते हैं - जो कि विरले ही देखने को मिलते हैं- वे व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। यदि मनुष्य के अन्दर श्रद्धा जागृत हो जाए तो वह पुरुषोत्तम के लिए कार्य करना आरम्भ कर देता है फिर चाहे उसके बाहरी प्रतीक बहुत सीमित, दोषपूर्ण और अपूर्ण ही क्यों न हों, क्योंकि आरम्भ में पूर्णता आना तो कठिन है। पर यदि व्यक्ति की भावना में, उसके विचारों या किसी एक हिस्से में शुद्धि है तो फिर सच्चा यज्ञ आरम्भ हो जाता है और इसके उत्तर में आती परमात्मा की चेतना व्यक्ति को इन चीजों से ऊपर उठा देती है। जो प्रतिफल देवताओं से प्राप्त होते हैं वे तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सहज सुलभ हो जाते हैं और उनका उसके लिये अधिक कोई मूल्य भी नहीं रह जाता। क्योंकि जब व्यक्ति में वह दूसरी चीज सक्रिय हो जाती है तब वह उस व्यक्ति की दृष्टि को इन सभी निम्न चीजों से बहुत ऊपर उठा ले जाती है, उसे अज्ञान से, मृत्यु से और संसार के बंधन से ऊपर उठा ले जाती है। फिर व्यक्ति निम्न आदान-प्रदान में लिप्त नहीं होता।
परन्तु यह प्राप्त करना सरल नहीं है। इसीलिए भगवान् सातवें अध्याय में कहते हैं कि जो लोग पितरों, गंधर्वो, यक्षों, देवताओं आदि की पूजा करते हैं वे उनके पास जाते हैं परन्तु जो मुझे पूजते हैं ऐसे मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। यदि व्यक्ति इस स्थिति तक पहुँच चुका है कि वह पुरुषोत्तम के प्रति, भगवान् के समग्र व्यक्तित्व के प्रति अभीप्सा कर सके, उनके लिए कर्म कर सके, तो जितना ही अधिक कुशलता से वह यह कर सकेगा उतना ही अधिक उसका अभ्युदय होगा। इस पूरे प्रकरण का हम यह अर्थ लगा सकते हैं। अन्यथा तो सामान्यतया व्यक्ति अपने-अपने तरीके से कर्म करते ही हैं और तदनुसार उन्हें उसका प्रतिफल भी प्राप्त होता है। जितना ही अधिक कोई व्यक्ति असंस्कृत होगा, असभ्य होगा, जिसके हेतु गलत होंगे, भावनाएँ अशुद्ध होंगी उसी hat vec m अनुसार उसके कर्म और प्रतिफल होंगे। इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। ये सभी देखने के तरीके मात्र ही हैं, इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ गीता का जो संदेश है वह गूढ़ है, और सतही तौर पर वह सहज ही प्रकट नहीं होता।
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम् ।। १३ ।।
१३. गुणों के और कर्मों के विभाग के अनुसार चातुर्वर्ण्य व्यवस्था मेरे द्वारा सृष्ट की गई है; यद्यपि मैं इन (चतुर्वर्ण विधान) की सृष्टि करने वाला हूँ तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जान।
केवल इसी उक्ति के बल पर ही सर्वथा यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि गीता इस प्रणाली को एक सनातन एवं सार्वभौम सामाजिक व्यवस्था के रूप में मानती थी। अन्य प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ इसे इस प्रकार नहीं मानते थे, उल्टे वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आदिकाल में इसका अस्तित्व नहीं था तथा विकास के उत्तर काल में इसका अंत हो जाएगा। तथापि इस उक्ति से हम यह समझ सकते हैं कि सामाजिक मनुष्य के चतुर्विध क्रिया-व्यवहार को प्रायः प्रत्येक समाज की मनोवैज्ञानिक और आर्थिक आवश्यकताओं में सामान्य रूप से अंतर्निहित ही माना जाता था और अतएव इसे परमात्मा का विधान समझा जाता था जो कि मानव के समष्टिगत एवं व्यष्टिगत जीवन में अपने-आप को अभिव्यक्त करता है।
....समाज की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था किसी ऐसे आध्यात्मिक सत्य का एक स्थूल या मूर्त रूप मात्र है, जो स्वयं उस स्थूल रूप से स्वतंत्र है। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि जिसके द्वारा कर्म किया जाता है उस कर्ता के स्वभाव की सम्यक् रूप से सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति के रूप में उचित कर्म संपादित हों और वह स्वभाव कर्त्ता के सहज गुण और आत्म-प्रकटनकारी वृत्ति के अनुसार उसके जीवन की धारा और क्षेत्र को निर्धारित करे।
VII
श्रीअरविन्द ने गुणों और कर्मों के विषय में 'स्वभाव और स्वधर्म' के अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। वे बता रहे हैं कि न ही ये हमेशा थे और न ही हमेशा रहने वाले हैं। किसी एक समय में ये उपयुक्त बन जाते हैं और किसी दूसरे समय में अप्रासंगिक। अब प्रश्न यह है कि ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था क्या है और इसका औचित्य क्या है? पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि सतयुग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी एक समान ही वर्ण के लोग थे जो परमात्मा की ओर अभिमुख थे। उन्हें हम द्विज, ब्राह्मण आदि कोई भी संज्ञा दे सकते हैं। अन्य कोई दूसरा वर्ण नहीं था। सतयुग एक ऐसा ही आदर्श समय था। तब फिर इन वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई? जगदम्बा की जब इस पृथ्वी पर अभिव्यक्ति हुई तो यद्यपि उनकी अनन्त शक्तियाँ और असंख्य व्यक्तित्व हैं, पर उनमें से उनकी चार महाशक्तियाँ - महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती - ही प्रधान रूप से अभिव्यक्त हुईं हैं और कार्य कर रही हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब वह अज्ञान से ढका होता है, और ज्यों-ज्यों वह विकसित होता है त्यों-त्यों ही उसकी विशिष्टता का, उसकी संभावनाओं का, उसकी रुचियों का स्पष्ट बोध होने लगता है। कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी में अमुक विशेषता होती है तो किसी में अन्य कोई गुण प्रधान होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वाँ बच्चों के भी गुण, चारित्रिक लक्षण, उनके रुझान भिन्न-भिन्न होते हैं। बाहरी रूप से पता नहीं चल सकता कि किसके लिए क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त।
भारतीय संस्कृति में एक समय ऐसा था जब इन चार महाशक्तियों की क्रिया के अनुरूप मनुष्यों के चार विस्तृत विभाजनों का बोध था और साथ ही यह बोध था कि किसी व्यक्ति में किसी एक या अधिक महाशक्तियों का प्राधान्य होने पर भी वास्तव में ये चारों ही शक्तियाँ व्यक्ति में विद्यमान होती हैं। किसी भी शक्ति से आरंभ कर के व्यक्ति अन्त में इन चारों ही शक्तियों का पूर्ण रूप से विकास करने पर श्रीमाताजी के (भगवान् के) मद्भाव में जा सकता है। इन सभी शक्तियों का यही हेतु है। परन्तु जब व्यक्ति आरंभ करता है तब वह अज्ञान से आच्छादित होता है और उसे अपने विषय में, अपने स्वभाव आदि के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। भारतीय व्यवस्था में यह बोध था कि व्यक्ति का जो मूलभूत स्वभाव है उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अर्थात् उसके कर्म ऐसे होने चाहिये जिसमें कि व्यक्ति के स्वभाव को अभिव्यक्ति मिल सके। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के स्वभाव में यदि महेश्वरी की प्रधानता हो पर उसे व्यापार करने में लगा दिया जाए तो यह उसके लिए विषमता की स्थिति पैदा कर देगा क्योंकि यह उसके स्वभाव के अनुरूप काम नहीं होगा। और इस कारण अपने सच्चे स्वभाव का बहुत क्षीण-सा अंश ही वह उसके अंदर अभिव्यक्त कर पाएगा। या फिर, जिस व्यक्ति में महाकाली की क्रिया की प्रधानता हो, उसे सेवा के कार्य में या फिर व्यापार में नियोजित कर दिया जाए, तो उसे वह कार्य अपनी प्रकृति के अनुकूल नहीं लगेगा। उसके स्वभाव में तो युद्ध करने, शासन करने आदि की शक्ति और संकल्प होता है। इसमें कार्य के अच्छे या बुरे होने का प्रश्न नहीं है। पर अपने स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण व्यक्ति उस कार्य के प्रति अरुचि रखता है। इसलिए हमारी संस्कृति में यह ज्ञात था कि स्वभाव नियत कर्म होना चाहिये। व्यक्ति को कर्म उसके स्वभाव के अनुरूप मिलना चाहिए। कुछ के स्वभाव का संतुलन ऐसा हो सकता है कि चारों ही शक्तियाँ उनमें क्रिया कर सकती हों, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी कर्म कर सकते हैं। परन्तु अधिकांश लोगों में ऐसा नहीं होता। इसलिए भारत में ये चार विस्तृत विभाजन थे और भगवान् यह कह रहे हैं कि ये विभाजन स्वयं उन्होंने ही किए हैं और इससे व्यक्ति को इसकी स्वीकृति मिल जाती है कि स्वभाव नियत कर्म ही करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर हजारों तरीके की शक्तियाँ हो सकती हैं पर ये चार मोटे तौर पर विभाजन किये गए हैं। जैसे कि, यदि व्यक्ति में ज्ञान प्राप्ति की उत्कण्ठा है और वह सत्य का पता लगाना चाहता है तो सत्य के अन्वेषण में अनेकानेक प्रकार के मार्ग होते हैं, अनेक तरीके की मनोवृत्तियाँ हो सकती हैं। परन्तु व्यक्ति को यदि स्वतंत्र अधिकार हो तो वह धीरे-धीरे कुछ चीजों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर के अपने मार्ग का पता लगा लेता है। सामान्य मार्गदर्शन के लिए ये चार विस्तृत विभाजन किए गए और उनके अन्दर भी चयन के बहुत विकल्प हैं, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को किस समय कैसा काम करना चाहिए यह प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। और व्यक्ति अपनी प्रेरणा, भावना, संकेतों और सुझावों के आधार पर आगे बढ़ता रहता है। केवल मोटे तौर पर समझने के लिए ही चार विभाजन किए गए हैं। पहला विभाजन ज्ञान से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति यह जानना चाहता है कि सत्य क्या है। उसे हम ब्राह्मण की संज्ञा देते हैं। दूसरा है क्षत्रिय जिसमें शक्ति की प्रधानता होती है जो केवल न्यायपूर्ण और उचित आचरण और कार्य-व्यवहार को श्रेष्ठ मानता है और अन्याय, अत्याचार और अनुचित के विरुद्ध लड़ता है। वह सत्य के लिए लड़ता है न कि अपने परिवार या सुख के लिए, भले उसे युद्ध में मरना ही क्यों ना पड़े। तीसरा विभाजन महालक्ष्मी का कार्यक्षेत्र है जिसमें व्यक्ति को मनुष्यों के बीच, चीजों के बीच, पशुओं के बीच आपसी तालमेल, प्रकृति के अंदर समन्वय और उचित व्यवस्था तथा पद्धति का बोध होता है। उदाहरण के लिए, यह बोध कि खेती करने का उचित तरीका क्या है, पशुओं का उचित रख-रखाव कैसे करना चाहिए, व्यापार को समुचित रूप से कैसे चलाना चाहिए, किसी भी चीज का सही रूप से निर्माण कैसे करना चाहिये। इन सब चीजों के उचित विधान महालक्ष्मी प्रदान करती हैं। जिस व्यक्ति में यह महालक्ष्मी की शक्ति होती है, वह समन्वय और संतुलन का ज्ञान रखता है, भौतिक वस्तुओं को कैसे संभालना या प्रयोग करना है, यह बोध रखता है। चौथे प्रकार के व्यक्ति में महासरस्वती की शक्ति होती है जिसके प्रभाव से वह छोटे-छोटे ब्यौरे की चीजों, जैसे कि हाथ की कारीगरी आदि, में कुशल होता है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति को अमुक प्रकार का भोजन चाहिए तो उसके लिए यह बोध कि इसमें फलां चीज मिलानी चाहिए, इतनी चीज मिलानी चाहिए, और तैयार होने के बाद किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति को वह भोजन मिल जाये, यह उद्योग महालक्ष्मी का है। परंतु भोजन को पकाना कैसे है, कौनसे मसालों का, किस मात्रा में प्रयोग करना है, वह सब ब्यौरेवार तैयारी करना और उसे क्रियान्वित करना महासरस्वती का कार्यक्षेत्र है। वास्तव में तो कार्य को संपूर्ण रूप से सिद्ध करने में चारों ही शक्तियों की आवश्यकता होती है। परंतु यह कार्य पर निर्भर करता है कि चारों में से प्राधान्य कौनसी शक्ति का होगा। इनमें सबसे बड़ी हैं महेश्वरी, क्योंकि सबसे पहले तो यह बोध होना आवश्यक है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। विना इस मोटी रूपरेखा के कोई भी कार्य आरंभ ही नहीं किया जा सकता। एक बार जब रूपरेखा तैयार हो जाए तब उसके लिए शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि महाकाली प्रदान करती हैं। उसके बाद उस कार्य के संपादन में विभिन्न घटकों में सही संतुलन और समन्वय स्थापित करने का कार्य महालक्ष्मी करती हैं, और अन्त में उस कार्य के ब्यौरों में पूर्णता लाना महासरस्वती का कार्यक्षेत्र है। इस प्रकार इन चारों शक्तियों के सहयोग से ही कोई कार्य पूर्ण रूप से सम्पन्न हो पाता है। ये चारों ही शक्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहती हैं। परंतु व्यक्ति में जिस भी शक्ति की प्रधानता होती है, उसी के अनुरूप कार्य में उसकी रुचि होगी और उसी में वह अधिक सफल हो पाएगा। यह सब आन्तरिक स्वभाव पर निर्भर करता है, अन्य किसी चीज पर नहीं। एक ही परिवार में हमें चारों वर्ण भी देखने को मिल सकते हैं। प्राचीन समय में भिन्न स्वभावों का बोध होने के कारण ही व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप व्यवस्था की जाती थी। परन्तु जब कालांतर में यह आंतरिक बोध क्षीण होता गया तब आंतरिक स्वभाव की बजाय जन्म को ही वर्ण का आधार माना जाने लगा। आज के समय में वह व्यवस्था अपना प्राचीन विशुद्ध स्वरूप खो बैठी है। उस व्यवस्था को अब हम भ्रमवश वर्तमान व्यावसायिक श्रेणियों की व्यवस्था समझ बैठते हैं। हालाँकि हर मनुष्य अपने अन्दर से महसूस कर लेता है कि उसके लिए कौनसा कर्म करना उचित है और कौनसा नहीं। और यदि वह किसी ऐसे कार्य में संलग्न होता है जो उसके स्वभाव के अनुरूप न हो तो अधिक समय तक वह उसे नहीं कर पाएगा और देर-सवेर उसे वह कार्य छोड़ना पड़ेगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए व्यापार उपयुक्त नहीं होता। कुछ दूसरे ऐसे हैं जिनके लिये कृषिकार्य उपयुक्त नहीं होता। वहीं, यदि किसी की प्रकृति ज्ञान की हो तो दूसरे कर्म उसे रास नहीं आते। इसी प्रकार सेवा करने की भी हर किसी की सामर्थ्य नहीं होती। प्रत्येक कार्य को दक्षतापूर्वक और ब्यौरेवार पूर्णता के साथ हर एक नहीं कर सकता। इसलिए चूंकि व्यक्तियों के आंतरिक स्वभाव भिन्न-भिन्न होने के कारण आंतरिक रूप से वह व्यवस्था पूर्ववत् ही प्रभावी है परंतु अभिव्यक्ति में वे चार विस्तृत विभाजन अब और अधिक प्रचलन में नहीं हैं। इस सब में भगवान् भीतर से मार्गदर्शन करते रहते हैं और वे मनुष्य को सही कार्य की ओर, सही स्थान पर और सही संपर्क में ले ही जाते हैं।
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ।। १४।।
१४. कर्म मुझ पर लिप्त नहीं होते (अपना प्रभाव नहीं छोड़ते) न ही मेरी कर्म के फल में कामना ही है; इस प्रकार जो मनुष्य मुझे जानता है वह अपने कमाँ से बद्ध नहीं होता।
मनुष्यों को... अपने स्वभाव (गुण) और कर्म के अनुसार चतुर्विध धर्म का पालन करना पड़ता है और सांसारिक कर्म के इस क्षेत्र में वे भगवान् को उनके विविध गुणों द्वारा ही ढूँढ़ते हैं। परन्तु श्रीकृष्ण कहते हैं कि यद्यपि मैं चतुर्विध कर्मों का कर्ता और चातुर्वर्ण्य का स्रष्टा हूँ तो भी मुझे अकर्ता, अविनाशी, अक्षर-आत्मा भी जानना चाहिए। "कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न कर्मफल की मुझे कोई स्पृहा है", क्योंकि भगवान् इस अहंभावापन्न व्यक्तित्व से तथा प्रकृति के गुणों के इस द्वन्द्व से परे निर्गुण-निर्वैयक्तिक हैं, और अपने पुरुषोत्तम-स्वरूप में भी, जो उनका निर्वैयक्तिक व्यक्तित्व है, वे कर्म के अन्दर रहते हुए भी अपनी इस परम स्वतंत्रता से संपन्न होते हैं। इसलिए दिव्य कर्मों के कर्त्ता को चातुर्वर्ण्य का पालन करते हुए भी जो परे है, निर्वैयक्तिक आत्मा में है और इसलिए परमेश्वर में है, उसी को जानना और उसी में निवास करना होता है। इस प्रकार "जो मुझे जानता है, वह अपने कर्मों से नहीं बँधता..."
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।
कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ।। १५।।
१५. ऐसा जानकर ही पूर्वकालीन मुमुक्षुओं द्वारा कर्म किया गया था; इसलिये तू भी प्राचीनकालीन पुरुषों के द्वारा किये हुए उस अतिप्राचीन प्रकार के कर्म को ही कर।
इसमें भगवान् ने अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि समस्त त्रिलोकी में उन्हें कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है परंतु फिर भी वे कर्म में रत रहते हैं। पुरुषोत्तम को न तो कर्म का बंधन होता है और न ही कामना का, और जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है वह कर्मों में नहीं बँधता। भगवान् किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करते। और यह निश्चित है कि कर्म के पीछे जिस प्रकार का फल हम चाहते हैं उसके लिये भगवान् कर्म नहीं करते। और जो व्यक्ति यह जानता है कि भगवान् कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते वह कर्मों से बद्ध नहीं होता क्योंकि वह तो केवल भगवान् के लिए ही कर्म करेगा। इस प्रकार के कर्म कर के बहुत लोग पवित्र हो चुके हैं।
अब प्रश्न यह उठता है कि जो व्यक्ति भगवान् के लिए कर्म करना चाहता है उसकी क्या विशेषताएँ या गुण हैं। अब चर्चा यह है कि दिव्य कर्मी जो यह जान जाता है कि किस प्रकार कर्म भगवान् को बाँधते नहीं, और कर्म में लिप्त न होते हुए भी भगवान् किस प्रकार कर्म करते हैं, वह कर्मी किस प्रकार कर्म करता है और उसकी क्या पहचान है? तब तक व्यक्ति में असमता होती है जब तक वह अपनी इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। परन्तु जब उसके मन में कोई कामना ही न रहे और वह केवल भगवान् की प्रसन्नता के लिये ही कर्म करता हो तब कार्य की सफलता और असफलता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सच्चे दृष्टिकोण से तो सभी कर्मों में सर्वदा भगवान् का संकल्प ही संसिद्ध होता है। और इस कारण समता स्वतः ही आ जाती है। इन सब बातों का स्पष्टीकरण अब आएगा।
II. दिव्य कार्यकर्त्ता
दिव्य जन्म को प्राप्त होना, जीव का एक उच्चतर चेतना में उठकर दिव्य बना देने वाले नवजन्म को प्राप्त होना, और दिव्य कर्म करना, नवजन्म सिद्ध होने से पहले साधन के तौर पर और वह सिद्ध हो जाने के बाद उसकी एक अभिव्यक्ति के तौर पर, यही गीता का संपूर्ण कर्मयोग है। गीता ऐसे किन्हीं बाह्य लक्षणों से कर्म को निरूपित करने का प्रयास नहीं करती जिनके द्वारा एक बाह्य दृष्टि के लिए यह पहचाने जाने योग्य हो सके, या लौकिक आलोचना-दृष्टि के लिए परिमेय अथवा थाह पाने योग्य हो सके, यह तो जान-बूझकर सामान्य नीतिधर्म के उन विशिष्ट लक्षणों को भी त्याग देती है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी मानव-बुद्धि के प्रकाश में (कर्तव्याकर्तव्य के लिए) अपना मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। गीता जिन लक्षणों से दिव्य कर्म की पहचान कराती है वे गहन रूप से आंतरिक और आत्मपरक हैं; जिस लक्षण या चिह्न से वे पहचाने जाते हैं वह अलक्ष्य, आध्यात्मिक और परा-नैतिक है। वे केवल उस आत्मा के प्रकाश द्वारा ही पहचाने जा सकने योग्य हैं जिससे कि वे उद्भूत होते हैं।
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ।। १६ ।।
१६. कर्म क्या और अकर्म क्या है इस विषय में कवि (ऋषि अथवा ज्ञानी पुरुष) भी भ्रान्त एवं मोहित हैं। उस कर्म को मैं तुझे बतलाऊँगा जिसे जानकर तू सम्पूर्ण अनिष्टों से मुक्त हो जाएगा।
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्व बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।। १७।।
१७. व्यक्ति को कर्म के स्वरूप को जानना चाहिये और विकर्म अर्थात् विपरीत कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिये और अकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिये; क्योंकि कमाँ का मार्ग घने वन के समान और उलझन वाला है।
-----------------------------------------
'झेलता मैं समान भाव से इस धरा की घटनाओं को;
सभी में सुनाई देती तेरे कदमों की आहट तेरे अगोचर चरण
मेरे सम्मुख नियति के पथों पर करते प्रयाण। जीवन के संपूर्ण
विशाल सूत्र का तुम ही हो पूर्णांग।
कर न सकता कोई संकट विचलित मेरी आत्मा की स्थिरता कोः
मेरे कर्म तेरे हैं; करता मैं तेरे कार्य और आगे निकल जाता;
असफलता सहारा पाती तेरी अमर भुजाओं में,
सफलता भाग्य के दर्पण में प्रतिबिंबित तेरा मार्ग है।
मानव के भाग्य से इस भीषण संघर्ष में
हृदयस्थ तेरी मुस्कान देती मुझे समस्त बल;
मुझमें तेरी शक्ति कार्यरत है अपनी विराट् योजना हेतु,
काल-सर्प की लंबी मंदगति से अप्रभावित
कोई शक्ति नहीं जो हत कर सके मेरी आत्मा को,
जो करती तुझमें निवास तेरी उपस्थिति ही है मेरी अमरता।
-श्री अरविन्द
संसार में कर्म एक गहन जंगल के समान है, जिसमें मनुष्य अधिक-से- अधिक अपने काल के विचारों, अपने व्यक्तित्व के मानदण्डों और अपने परिवेश के अनुसार ठोकरें खाता हुआ चलता है; या यों कहें कि वह चलता है अनेक कालों के विचारों, अनेक व्यक्तित्वों के मानदण्डों और अनेक सामाजिक अवस्थाओं के नैतिक-धर्मों के अनुसार जो कि एक दूसरे से अस्तव्यस्तता में घनिष्ठ रूप से मिले हुए हैं, जो अपने समस्त निरपेक्ष और अविनाशी होने के दावे के बावजूद भी तात्कालिक और रूढ़िगत ही होते हैं, और युक्तिपूर्ण होने का दिखावा करने के बावजूद अशास्त्रीय और अयौक्तिक ही होते हैं। और अंततः, इस सबके बीच सुनिश्चित कर्म-विधान के किसी महत्तम आधार और मूल सत्य को ढूँढ़ता हुआ ज्ञानी अंत में अपने-आप को इस चरम प्रश्न को उठाने के लिए बाध्य पाता है कि कहीं यह सारा कर्म और स्वयं जीवन भो केवल एक भ्रम तथा एक जाल-फाँस तो नहीं है और कहीं इस क्लांत और भ्रान्ति-मुक्त मानव-जीव के लिए कर्म का परित्याग कर अकर्म अपनाना ही अंतिम आश्रय तो नहीं है। परन्तु श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस बारे में ज्ञानी भी भ्रमित और मोहित हो जाते हैं। क्योंकि क्रिया द्वारा, कर्मों द्वारा, न कि अकर्म द्वारा, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
'संसार में कर्म एक गहन जंगल के समान है, जिसमें मनुष्य अधिक-से-अधिक अपने काल के विचारों, अपने व्यक्तित्व के मानदण्डों और अपने परिवेश के अनुसार ठोकरें खाता हुआ चलता है;' जव व्यक्ति कर्म करता है तब उसके मन में अनेकानेक विचार तथा प्रश्न उठते हैं कि कौन-सा कर्म करना चाहिए, कौन-से कर्म में फायदा है, किस कर्म में सुख मिलेगा। कर्म के चयन करने का यह एक आधार है। और दूसरा यह कि व्यक्ति के मन में आता है कि अमुक कर्म करना ठीक है पर उसको लगता है कि वह दूसरा कर्म करना भी ठीक है। इन विचारों के बाद अब वह सोचता है कि इनमें से एक कर्म करना तो संभव है पर दूसरा करना तो असंभव है या फिर अधिक मुश्किल है क्योंकि उसके लिए तो इन-इन चीजों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त मनुष्य के सामने एकाएक ही कोई सुअवसर भी आ सकता है और व्यक्ति अपने हाथ के कार्य को छोड़कर उसमें लग जाता है। अधिकांशतः इसी तरह मनुष्य अपने कर्मों का चुनाव करते हैं और इस चुनाव में व्यक्ति की परिस्थिति, वातावरण, परिवेश, विचार, भावना और लोगों के साथ उसके संबंधों की भी भूमिका रहती है। इनके साथ-ही-साथ सदा ही यह संभावना भी रहती है कि कोई अप्रत्याशित सुअवसर या संयोग प्राप्त हो जाए और वह इन सब से छूटकर किसी अन्य कर्म का चुनाव कर ले। इस तरीके के कर्म का जंगल इस संसार में है। 'या यों कहें कि वह चलता है अनेक कालों के विचारों, अनेक व्यक्तित्वों के मानदण्डों और अनेक सामाजिक अवस्थाओं के नैतिक-धर्मों के अनुसार जो कि एक दूसरे से अस्तव्यस्तता में घनिष्ठ रूप से मिले हुए हैं,' कर्मों के निर्णय में भी कोई एक ही नियत-निर्धारित विचार या मानदंड नहीं है, पारंपरिक या शास्त्र-सम्मत विचारों के आधार पर भी एक व्यक्ति कर्म करने का एक तरीका बताता है और दूसरा व्यक्ति दूसरा, तो इस प्रकार हजारों तरीकों के परस्पर पूरक या विरोधी विचार आकर उपस्थित हो जाते हैं। हमारे अपने मन में भी उथल-पुथल चलती रहती है और अनेकानेक तरीके के विचार गुजरते रहते हैं और साथ ही यह भी तय नहीं है कि किस समय किस प्रकार का सुअवसर आ जाए। यह सारा मेलजोल चलता रहता है और यह मेलजोल भी केवल किसी अवधि विशेष का ही नहीं बल्कि इसमें पूर्वजन्मों की व भूतकाल की घटनाओं और भविष्य की प्रत्याशाओं और वर्तमान जीवन और विचारों की मिलावट होती रहती है। इसके अतिरिक्त इसमें व्यक्ति की आकांक्षा, भय, कामना आदि हजारों चीजों का मिश्रण चलता रहता है क्योंकि हजारों तरीके की शक्तियाँ होती हैं जो हमें अपने उपयोग में लेना चाहती हैं, और जिस समय जिस शक्ति को अवसर मिल जाता है वही हमें अपने उपयोग में ले लेती है। और इस सब प्रकार के भ्रम या भ्रांति में मनुष्य कर्म करता रहता है जिसका आसानी से कोई ओर-छोर नहीं मिलता। इसीलिए मनुष्य पाता है कि वह सोच कर कुछ चलता है जबकि उसका परिणाम कुछ और ही निकलता है। इन आधारों से कर्म के जो निर्णय होते हैं उनसे सहज ही छुटकारा नहीं पाया जा सकता। यह बहुत ही जटिल विषय है। 'और अंततः, इस सबके बीच सुनिश्चित कर्म-विधान के किसी महत्तम आधार और मूल सत्य को ढूँढ़ता हुआ ज्ञानी अंत में अपने-आप को इस चरम प्रश्न को उठाने के लिए बाध्य पाता है कि कहीं यह सारा कर्म और स्वयं जीवन भी केवल एक भ्रम तथा एक जाल-फाँस तो नहीं है और कहीं इस क्लांत और भ्रान्ति-मुक्त मानव-जीव के लिए कर्म का परित्याग कर अकर्म अपनाना ही अंतिम आश्रय तो नहीं है।' अगर व्यक्ति के मन में यह भाव आ भी जाए कि इन कर्मों से वह ऊपर उठ जाएगा, भगवान् की ओर चलेगा या फिर पूर्णता के मार्ग पर चलेगा और उसके लिये वह प्रयास भी करता है, तब भी वह पाता है कि वह अपने कर्मों में फँसता ही है, कुछ भी करने से कोई उपाय नहीं निकलता है। व्यक्ति जब साधना-मार्ग में होता है तब आरंभ में वह देखता है कि जब तक वह केवल भगवान् का भजन करता है और कर्म कम-से-कम ही करता है तब तक तो वह कुछ हद तक भगवान् पर केंद्रित रह पाता है परन्तु जैसे ही वह कोई व्यावहारिक कर्म करता है, या किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आता है जो इस मार्ग पर नहीं हैं तो उसकी चेतना में गिरावट आती है जिसके कारण साधना से भिन्न बातें मन में आने लगती हैं। इसलिये कर्मों को करने से ऐसा लगता है मानो कर्म करना योग नहीं बल्कि एक प्रकार का रोग है। इससे तो अच्छा है कि संसार से अपने-आप को हटा के शान्ति से रहा जाए, भगवान् का ध्यान किया जाए, उनकी चेतना से जुड़ा जाए, और फिर समय पाकर जब नश्वर शरीर नष्ट हो तो हो जावे। जो लोग साधना करते हैं उनमें सामान्यतः तो यह धारणा प्रत्यक्ष या अप्रकट रूप में अंदर होती ही है। परन्तु यह सब करने पर भी व्यक्ति पाता है कि वास्तव में इस समस्या का समाधान नहीं होता। यहाँ तक कि जो लोग साधना मार्ग में हैं उन्हें भी अलग-अलग मात्रा में अपनी-अपनी शिकायतें रहती हैं। और इस सब से थक कर अन्त में व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह सब प्रपंच ही मिथ्या है और इस प्रकार वह भ्रम में पड़ जाता कि क्या किया जाए क्योंकि कर्म करने के साथ ही प्राण अपनी क्रिया चालू कर देता है और जब तक व्यक्ति इसके विषय में सचेत हो पाता है तब तक तो बहुत समय निकल चुका होता है। और उससे निकल कर व्यक्ति निश्चय करता है कि अब वह अधिक सचेत रहने का प्रयास करेगा पर कुछ ही समय बाद वह पाता है कि प्राण की अन्य कोई क्रिया चल रही है और वह उसमें फँसा हुआ है। इसलिए व्यक्ति को लगता है कि भले कोई भी कर्म कर लो पर कामनाओं से मुक्ति पाना तो संभव ही नहीं है। कोई न कोई सूक्ष्म हेतु तो चलता ही रहता है। इस तरीके से व्यक्ति कर्म के विषय में बहुत ही अधिक भ्रांति में पड़ जाता है कि आखिर करे क्या। 'श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस बारे में ज्ञानी भी भ्रमित और मोहित हो जाते हैं। क्योंकि क्रिया द्वारा, कमाँ द्वारा, न कि अकर्म द्वारा, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।'
इस बारे में श्रीकृष्ण कहते हैं कि शुरू में व्यक्ति के कर्म ऐसे होने चाहिए जो उसे परमात्मा की ओर ले जाएँ। और एक बार जब व्यक्ति भगवान् से जुड़ जाए तो उनकी प्रेरणा के अनुसार सारे कर्म करने चाहिये। श्रीमाताजी जो कर्म कराएँ वे ही करने चाहिये। उन कर्मों की पहचान कैसे हो और उन्हें संपादित कैसे किया जाए, इन सब प्रश्नों की चर्चा गीता आरम्भ से ही कर रही है और साथ ही उसमें नए तत्त्व भी जोड़ती जा रही है कि ज्ञान कर्मों को आगे बढ़ाता है और कर्म करने से ज्ञान और अधिक बढ़ता है और ज्ञान में वृद्धि कर्मों में सुधार लाती है। यह क्रम चलता रहता है और जब श्रीमाताजी के प्रति भक्ति आ जाती है तब इनमें एक विशेष तत्त्व सम्मिलित हो जाता है। भक्ति के आने से कमों में और अधिक शुद्धि आ जाती है। ये सारी बातें गीता हमें धीरे-धीरे समझा रही है। इस प्रकार गीता का सारा विकासक्रम बिल्कुल संबद्ध तरीके से और युक्तियुक्त तरीके से चल रहा है। आरंभ में वह निष्काम कर्म के विषय में बताती है। और जब प्रश्न यह उठता है कि निष्काम कर्म करें कैसे तब उसके उत्तरस्वरूप वह कहती है कि भगवान् की प्रसन्नता के निमित्त कर्म करो। उसके बाद वह इसकी व्याख्या करती है कि ज्ञान और कर्म का क्या संबंध है। यह व्याख्या करने के बाद वह यह चर्चा करती है कि दिव्यकर्मी की स्थिति कैसे प्राप्त हो जो लाभ-अलाभ में, जय-पराजय में और सफलता-असफलता में समान रहता है। उसके बाद इस रहस्य का निरूपण करती है कि यह समत्व कैसे प्राप्त होगा। धीरे-धीरे गीता इसमें भक्ति के तत्त्व को समाविष्ट करती है और उन प्रभु का स्वरूप बतलाती है जिनके प्रति यह भक्ति अर्पित करनी है। इस प्रकार सारा ही क्रम बिल्कुल संबद्ध रूप से चल रहा है।
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ।। १८ ।।
१८. जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और कर्मों के परित्याग में भी कर्म को होते हुए देखता है वह मनुष्यों में सच्ची बुद्धिवाला और विवेकयुक्त होता है; वह योगयुक्त होता है, और बहुमुखी विश्वव्यापी कर्म करनेवाला होता है।
तब समाधान क्या है? कर्म का वह कौन-सा प्रकार होगा जिसके द्वारा हम जीवन के अशुभ से छूट सकेंगे, इस संशय, त्रुटि और शोक से, अपने विशुद्धतम और श्रेष्ठतम हेतुओं से प्रेरित कर्मों के भी मिले-जुले, अशुद्ध और भ्रांतिजनक परिणाम से, इन लाखों-लाख प्रकार की बुराइयों और दुःखों से, मुक्त हो सकेंगे? उत्तर मिलता है कि कोई बाह्य विभेद करने की आवश्यकता नहीं, इस जगत् के किसी भी कार्य के परित्याग की आवश्यकता नहीं; हमारी मानव-गतिविधियों के चारों ओर कोई परिसीमा या बाड़ लगाने की आवश्यकता नहीं; इसके विपरीत, सभी कर्म किये जाने चाहिए, परंतु भगवान् के साथ योगयुक्त हुई आत्मा से, युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। अकर्म, अर्थात् कर्म का परित्याग, (सही) मार्ग नहीं है; जो व्यक्ति उच्चतम बुद्धि की अंतर्दृष्टि को प्राप्त हो गया है, वह देखता है कि इस प्रकार का अकर्म भी स्वयं सतत् होनेवाला एक कर्म है, एक ऐसी अवस्था है जो प्रकृति और उसके गुणों की क्रियाओं के अधीन है। जो मन शारीरिक अकर्मण्यता का आश्रय लेता है, वह अभी भी इसी भ्रम में है कि वह स्वयं कर्मों का कर्ता है, न कि प्रकृति; उसने जड़ता या निष्क्रियता को मोक्ष समझ लिया होता है; वह यह नहीं देखता कि जो पत्थर या ढेले की जड़ता से भी अधिक चरम जड़ता प्रतीत होती है उसमें भी प्रकृति क्रियारत होती है, उस पर भी प्रकृति अपना अक्षुण्ण अधिकार रखती है। इसके विपरीत, कर्म की विपुल बाढ़ में भी आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होती है, वह कर्ता नहीं होती, जो कुछ किया जा रहा है उससे बाध्य नहीं होती, और जो आत्मा की मुक्तावस्था में निवास करता है न कि प्रकृति के गुणों के बंधनों में, उसी को कर्मों से मुक्ति मिलती है। यही स्पष्टतः गीता का आशय होता है जब वह यह कहती है कि 'जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वही मनुष्यों में विवेकी और बुद्धिमान् है।' यह कथन सांख्य द्वारा पुरुष और प्रकृति के बीच किये भेद पर, अर्थात् कर्मों के बीच भी शाश्वत रूप से प्रशांत, शुद्ध और अचल मुक्त निष्क्रिय आत्मा के तथा नित्य क्रियाशील प्रकृति - जो जड़ता और अकर्मण्यता में भी उतनी ही कार्यरत है जितनी कि उसके घोर कर्म की गोचर आकुलता के प्रत्यक्ष उत्पात में- के बीच किये भेद पर आधारित है। यही वह उच्चतम ज्ञान है जो बुद्धि का उच्चतम प्रयास हमें प्रदान करता है, और इसलिए जो कोई भी इस ज्ञान को अधिकृत रखता है वही यथार्थ में बुद्धिमान् है, 'स बुद्धिमान् मनुष्येषु', - न कि कोई ऐसा भ्रान्त या मोहित बुद्धिवाला मनुष्य जो जीवन और कर्म की परख निम्नतर बुद्धि के बाह्य, अनिश्चित और अस्थायी लक्षणों से करता हो। इसलिए मुक्त पुरुष कर्म से भयभीत नहीं होता, वह सभी कर्मों का करनेवाला विशाल और महत् कर्मी होता है (कृत्स्नकर्मकृत्)। वह औरों की तरह प्रकृति के वश में रहकर कर्म नहीं करता, अपितु आत्मा की नीरव स्थिरता में प्रतिष्ठित होकर, शांतिपूर्वक भगवान् के साथ योगयुक्त होकर कर्म करता है। भगवान् उसके कर्मों के स्वामी होते हैं, वह उन कर्मों का निमित्तमात्र होता है जो उसकी प्रकृति अपने स्वामी को जानते हुए, उन्हीं के वश में रहते हुए करती है।
इसमें यह स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि क्या कर्म है और क्या अकर्म तथा कौन कर्ता है और कौन अकर्ता। जो व्यक्ति कभी भी कोई कर्म नहीं करता, जो बिल्कुल पत्थर के समान निष्क्रिय रहता है, वह भी प्रकृति का दास है और उसकी क्रिया से नहीं बच सकता। भगवान् की परा प्रकृति के द्वारा ही यह समस्त अभिव्यक्ति होती है अतः इससे कोई नहीं बच सकता और इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह कुछ भी कर्म न कर के पत्थर की तरह जड़ होकर कर्मों से मुक्त हो जाएगा तो यह उसका भ्रम है। ऐसे व्यक्ति के अकर्म में भी घोर तामसिक प्रकार का कर्म होता है। वहीं कर्म के अंदर घोर रूप से संलग्न दिखाई देने पर भी संभव है कि व्यक्ति वास्तव में कोई कर्म न कर रहा हो क्योंकि वह जानता है कि कर्म तो भगवान् की शक्ति के द्वारा संपादित हो रहे हैं और प्रकृति के नियंता के साथ सतत् रूप से जुड़े होने के कारण उसके सारे कर्म प्रकृति के होते हैं और वह स्वयं उनसे मुक्त होता है। इसलिए वह कर्म करते हुए भी कर्मों से मुक्त होता है, उसके ऊपर कर्मों का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। और यही कर्मयोग का आधार है अन्यथा तो कर्म योग नहीं अपितु रोग स्वरूप ही होता है। जब तक व्यक्ति का भगवान् के साथ सतत् संपर्क साधित नहीं होता तब तक वह चाहे कर्म करे या न करे, अधिक करे या कम करे, वह कर्मरोगी ही होता है क्योंकि वह अपनी कामनाओं और इच्छाओं के लिए ही कर्म करता है। जब व्यक्ति पुरुषोत्तम के साथ एक होता है तभी वह कर्मों का स्वामी होता है अन्यथा तो वह उनका दास ही होता है। अक्षर पुरुष में स्थित होने पर तो व्यक्ति कर्मों से बिल्कुल दूर हट जाता है और वह कोई भी सृजनात्मक कार्य नहीं कर सकता क्योंकि अक्षर तो एक स्थिति है। उस स्थिति में व्यक्ति को जीवन में कर्म का कोई आधार प्राप्त नहीं होता। केवल पुरुषोत्तम के साथ एक होने पर ही व्यक्ति को कर्मों का आधार प्राप्त होता है। इसी स्थिति में व्यक्ति कर्मों को करने पर भी उनसे परे रहता है। इस प्रकार गीता ने कर्मों का समाधान बता दिया है कि यदि व्यक्ति भगवान् के साथ युक्त है तो उसके सारे कर्म बहुत अच्छे हैं और भगवान् उसकी सहायता कर रहे होते हैं और यदि व्यक्ति उनके साथ युक्त नहीं है तो वह कितने ही अधिक कर्म करे या न करे, वह अपनी इच्छाओं और कामनाओं से घिरा रहता है, उनमें लिप्त रहता है। इसलिए उसके सभी कर्म कर्म नहीं अकर्म ही होते हैं और यह एक प्रकार का कर्मरोग है। पर इसमें समस्या यह आती है कि व्यक्ति उस आदर्श स्थिति में एकाएक ही तो नहीं जा सकता इसलिए उसे कर्मरोग में से होकर ही गुजरना पड़ता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसके समाधान के रूप में यज्ञरूप कर्म का प्रतिपादन किया गया है। यज्ञ के द्वारा ही व्यक्ति कर्मरोग से कर्मयोग की ओर जा सकता है। वर्तमान प्रसंग में तो इसका वर्णन है कि जो व्यक्ति इससे मुक्त है उसके कर्म किस प्रकार के होते हैं।
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ।। १९।।
१९. जिसके सम्पूर्ण कर्मों के प्रारंभ और अनुष्ठान कामनायुक्त निम्न कोटि के संकल्प से रहित हैं, ज्ञानरूपी अग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो गये हैं; उसे ज्ञानी मनुष्य पण्डित कहते हैं।
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ।। २० ।।
२०. अपने कर्मों के फलों में आसक्ति का परित्याग कर के, किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहते हुए सदा संतुष्ट, वह अपनी प्रकृति के द्वारा कर्म में प्रवृत्त रहने पर भी (स्वयं) कुछ नहीं करता।
इस ज्ञान की प्रदीप्त गहनता और पवित्रता द्वारा उसके कर्म जला दिए जाते हैं जैसे कि अग्नि में जलकर भस्म हो गए हों और उसका मन इनके द्वारा किसी भी दाग या धब्बे से मुक्त, स्थिर, शान्त, अचल, निर्मल, शुभ और पवित्र बना रहता है। कर्तृत्व-अभिमान से शून्य इस मोक्षदायक ज्ञान में स्थित होकर समस्त कर्मों को करना ही दिव्य कर्मी का प्रथम लक्षण है।
दूसरा लक्षण है कामना से मुक्ति; क्योंकि जहाँ कर्ता का व्यक्तिगत अहंकार नहीं होता वहाँ कामना का रहना असंभव हो जाता है, वहाँ कामना भूखों मरने लगती है, बिना किसी आश्रय या प्रोत्साहन प्राप्त किये यह क्षीण हो जाती है और भरण-पोषण के अभाव में नष्ट हो जाती है। बाह्यतः मुक्त व्यक्ति भी दूसरे लोगों की तरह ही समस्त कर्मों को करता हुआ दिखायी देता है, कदाचित् वह कर्मों को बड़े पैमाने पर और अधिक शक्तिशाली संकल्प और वेगवती शक्ति के साथ करता है, क्योंकि उसकी सक्रिय प्रकृति में भागवत् संकल्प का बल काम करता है; परन्तु उसके समस्त उपक्रमों और उद्योगों में कामना के हीनतर भाव और निम्नतर इच्छा को सर्वथा निष्कासित कर दिया गया होता है, सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः। उसने अपने कर्मों के फल की समस्त आसक्ति का परित्याग कर दिया होता है, और जहाँ व्यक्ति फल के लिए कर्म नहीं करता अपितु केवल कर्मों के स्वामी के एक नैर्व्यक्तिक यंत्र के रूप में ही सारा कर्म करता है वहाँ कामना-वासना कोई स्थान ही नहीं पाती... मुक्त पुरुष का मानव-मन और अंतरात्मा कुछ भी नहीं करता, न किञ्चित् करोति; यद्यपि वह अपनी प्रकृति के द्वारा कर्म में प्रवृत्त तो होता है, पर कर्म करती है वह प्रकृति, वह की शक्ति, वह चिन्मयी भगवती जो दिव्य अंतर्वासी के द्वारा नियंत्रित होती है।
इसमें दो लक्षण बताए गए हैं। एक है ज्ञानाग्नि के द्वारा अहं भाव का नष्ट हो जाना और दूसरा लक्षण है, सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः, अर्थात् व्यक्ति का कर्म तो करना परन्तु उसमें किसी प्रकार की कामना का न होना। इस प्रकार - काम-संकल्प से मुक्ति और अहं से मुक्ति - दिव्य कर्मी के ये दो लक्षण बताए गए हैं। और भी कई प्रकार के लक्षण श्रीअरविन्द बताएँगे। परन्तु इन दोनों में एक तो यह है कि ज्ञानाग्नि व्यक्ति के अहं को दग्ध कर के मिटा देती है। और दूसरा यह कि व्यक्ति की कामनाएँ नष्ट हो गईं हैं और उसके सारे कर्म भगवान् की दिव्य प्रकृति को, भागवत् शक्ति को समर्पित हैं, और वह दिव्य प्रकृति ही उसके कर्म करती है। व्यक्ति की उनमें कोई लिप्तता नहीं होती। जैसे गीता में भगवान् ने कहा है कि 'कर्म तो केवल मेरी प्रकृति ही करती है, केवल मूढ़ जन ही ऐसा सोचते हैं कि कर्म वे स्वयं कर रहे हैं।' पहले तो गीता में कहा गया कि 'कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन' कि व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है परन्तु कर्मों को करने पर उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परंतु उसके बाद यह बता दिया कि कर्म तो भगवान् की परा शक्ति ही करती है। वही शक्ति कमर्मों का आरम्भ करती है और वही उसको पूरा करती है। और जो व्यक्ति इस रहस्य को जान जाता है कि कर्म का आरंभ, उसका संपादन और उसका समापन तो भगवान् की दिव्य प्रकृति करती है, उसमें फिर काम-संकल्प नहीं रह जाता। और इस स्थिति में अपने को कर्ता बताने का अहंभाव नहीं होता और अहंभाव न हो तो कामना स्वतः ही नहीं आएगी। कामना तो जड़ से ही समाप्त हो जाती है। कामना तो केवल इसलिए आती है क्योंकि व्यक्ति अपने-आप को अधूरा या अतृप्त महसूस करता है और यह सोचता है कि मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ इसीलिए वह कभी किसी चीज की इच्छा करता है, तो कभी किसी चीज से बचने का प्रयास करता है। परन्तु जब उसे यह भान हो जाता है कि उसके अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्माण्ड में अन्य किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है तब फिर वह कामना किस चीज की करेगा। ऐसी स्थिति आने पर कामना तो जड़ से ही समाप्त हो जाती है। कामना इसीलिए तो खराब बताई जाती है क्योंकि व्यक्ति जब भी कामना करता है तभी अपने अहं को, अपने पृथक् अस्तित्व को - कि वह अलग है और दूसरे लोग अलग हैं - बढ़ावा देता है और इसी पर आग्रह करता है। हर बार जब व्यक्ति किसी कामना से और अहंभाव से कर्म करता है कि 'मैं' यह कर्म कर रहा हूँ, 'मैं' अमुक चीज प्राप्त करना चाहता हूँ या अमुक चीज प्राप्त नहीं करना चाहता, तो हर बार इस 'मैं' 'मेरे' के अज्ञान की छाप लग जाती है जिससे बचने के उपायों की हम बात कर रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कामना का होना व्यक्ति को मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कामना तथा संकल्प या इच्छा-शक्ति में भेद है। इच्छा-शक्ति या संकल्प भिन्न चीज है। उसमें व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह ही सब कुछ है और वह चाहे जो कर सकता है। और सच्चा संकल्प तब आता है जब व्यक्ति भगवान् के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाता है। जब अपने-आप को एक पृथक् व्यक्तित्व मानकर व्यक्ति कुछ करने का प्रयत्न करता है तो यह कामना है। व्यक्ति में इन दोनों चीजों का मिश्रण चलता रहता है। परन्तु उसे इस चीज का बोध नहीं होता। जब व्यक्ति श्रीमाताजी के साथ युक्त हो जाता है तब उसके कर्म बाहरी रूप से चाहे कैसे भी प्रतीत क्यों न हों, पर वे भागवत् संकल्प द्वारा चालित होते हैं। उनमें कामना का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कर्म को पूर्णतः सम्यक् रूप से, सफलतापूर्वक, उपयुक्त साधनों को लक्ष्य के अनुरूप रखकर न किया जाएः इसके विपरीत, योगस्थ होकर शान्ति के साथ कर्म करने से कुशल कर्म करना जितना अधिक सुलभ होता है उतना आशा और भय से अंधे होकर या फिर अधीर मानव-इच्छा की उत्सुकतापूर्ण घबराहट के बीच दौड़-धूप करती डगमगाती बुद्धि के निर्णयों द्वारा लँगड़े बने हुए कर्मों को करने से नहीं होता। गीता अन्यत्र कहती है, योगः कर्मसु कौशलम्, कि योग ही है कर्म का सच्चा कौशल। परंतु यह सब होता है नैयक्तिक भाव से एक महती विश्व-ज्योति और शक्ति के द्वारा जो व्यष्टिगत प्रकृति के माध्यम से अपना कर्म करती है... कर्म का फल वैसा भी हो सकता है जिसे सामान्य मन सफलता समझता है, अथवा यह उस मन को पराजय और विफलता' भी प्रतीत हो सकती है, परंतु दिव्यकर्मी के लिए यह सदा ही अभीष्ट सफलता होती है, जो उसके अपने द्वारा अभिप्रेत या अभीष्ट नहीं होती, अपितु कर्म और फल दोनों के सर्वज्ञ संचालक के द्वारा होती है, क्योंकि वह (दिव्यकर्मी) विजय की खोज नहीं करता, अपितु केवल उस भगवत्संकल्प और प्रज्ञा की चरितार्थता के लिए यत्न करता है जो अपने लक्ष्यों की संसिद्धि जितनी ऊपरी रूप से दिखने में जो जय प्रतीत होती है उसके द्वारा करती है और उतनी ही और प्रायः उससे भी कहीं अधिक शक्ति के साथ जो दिखने में असफलता प्रतीत होती है उसके द्वारा करती है। अर्जुन को युद्ध के आदेश के साथ-साथ विजय का आश्वासन भी प्राप्त है; परंतु यदि उसके समक्ष निश्चित हार भी होती तो भी उसे अवश्य युद्ध करना है; क्योंकि जिन क्रियाशक्तियों के समूह के द्वारा भगवान् का संकल्प अवश्य सफल होता है उसमें तात्कालिक भाग के तौर पर अर्जुन को वर्तमान में यह युद्ध-कर्म ही सौंपा गया है।
यहाँ श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि 'योगः कर्मसु कौशलम्' अर्थात् योग ही कर्मों में कुशलता है। जब व्यक्ति अहंवश कर्म करता है तो न तो उसकी बुद्धि शांत होती है और न ही उसका चित्त शांत होता है और वह चिन्तातुर और उद्विग्न होकर कर्म करता है। वहीं, जब व्यक्ति योग करता है तो उसकी बुद्धि शांत-प्रशांत होती है। किसी भी प्रकार के कर्मों को करते हुए उसका हृदय विचलित नहीं होता। ऐसे कर्म में लोग जिसे सफलता कहते हैं वह भी उसके लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण होती है जितनी कि वह जिसे वे असफलता कहते हैं। इसलिए उसके सारे कर्म छोटे-से-छोटे ब्यौरे में भी पूर्णता के साथ निष्पादित होते हैं। 'योगः कर्मसु कौशलम्' का तात्पर्य किसी कुशल कारीगर या व्यापारी या फिर बढ़ई आदि से नहीं है जो अपने कर्मों को बड़ी कुशलता या निपुणता के साथ करता है। एक योगी ही है जो यह जानता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। विना योगयुक्त हुए व्यक्ति यह सब जान ही नहीं सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि बहुत बढ़िया कार से यात्रा कर रहा हो और कार चलाने में भी बहुत कुशल हो परन्तु गलत दिशा में जा रहा हो तो यह यात्रा की कुशलता नहीं हुई। यात्रा की कुशलता तो इस बात में है कि व्यक्ति इस विषय में सज्ञान हो कि कहाँ और कैसे जाना चाहिए। यह ज्ञान केवल योग के द्वारा ही आ सकता है। और इसमें केवल पता ही नहीं चलता अपितु कर्मों के संपादन की कुशलता भी योग से ही आती है। योगयुक्त का अर्थ है कि व्यक्ति दिव्य शक्ति के प्रति समर्पित होता है और उसके माध्यम से उस शक्ति की ही क्रिया होती है और उसके सारे कर्म उस शक्ति के द्वारा ही समुचित व पूर्ण रूप से निष्पादित होते हैं। ऐसे में व्यक्ति के अहं, उसकी वासनाओं, इच्छाओं, अस्थिरता आदि का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए योग की अवस्था में ही कर्म की सच्ची प्रेरणा और उसका पूर्ण रूप से सटीक निष्पादन संभव होता है। योग न केवल अपने-आप में श्रेष्ठ है अपितु कर्म-संपादन में भी वह श्रेष्ठ है। गीता का तो आरम्भ इसी से होता है जिसमें भगवान् अर्जुन को कहते हैं कि तू जय-पराजय, लाभ-हानि की चिन्ता किए बिना, मेरी प्रसन्नता के निमित्त कर्म करता हुआ युद्ध कर।
---------------------------------
'जिसका नेतृत्व 'प्रभु' करते हैं उसकी विफलता कोई विफलता नहीं….
फिर दिव्य कर्मी का लक्षण वह है जो स्वयं भागवत् चेतना का केन्द्रीय लक्षण है, अर्थात् पूर्ण आन्तरिक आनन्द और शान्ति की स्थिति जो इस जगत् के किसी भी पदार्थ पर अपने उद्गम और अपने निरंतर बने रहने के लिए निर्भर नहीं है; यह सहज अंतर्निहित होती है, यह अंतरात्मा की चेतना का तत्त्वमात्र होती है, दिव्य सत्ता की प्रकृतिमात्र ही होती है। सामान्य मनुष्य अपने सुख या प्रसन्नता के लिए बाह्य पदार्थों पर निर्भर रहता है; इसी से उसमें कामना होती है; इसी से उसमें क्रोध-आवेश, सुख-दुःख, हर्ष-शोक होते हैं; इसीलिए वह सब वस्तुओं को सौभाग्य-दुर्भाग्य के तराजू में तौलता है। परन्तु इनमें से कोई भी चीज दिव्य आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती; किसी भी प्रकार की पराश्रितता के बिना यह नित्य-तृप्त रहती है, नित्यतृप्तो निराश्रयः, क्योंकि उसका आनन्द, उसका दिव्य सुख, उसकी प्रसन्नता, उसकी हर्षित ज्योति सदा उसके अन्दर शाश्वत रूप से निहित हैं, उसमें स्वयं में अंतर्व्याप्त हैं. ... सभी पदार्थों में वह एक ही समान अक्षय आनन्द लाभ करता है...
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ।। २१ ।।
२१. वह व्यक्तिगत आशा (कामना) से रहित होता है, उसके हृदय और अन्तःकरण पूरी तरह संयत रहते हैं, वह वस्तुओं को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर ग्रहण नहीं करता, केवल शारीरिक कर्म करता हुआ वह पाप को प्राप्त नहीं होता।
मुक्त पुरुष की व्यक्तिगत आशाएँ-आकांक्षाएँ नहीं होतीं; वह चीजों को अपनी वैयक्तिक संपत्ति जानकर नहीं पकड़े रहता, भगवत्संकल्प जो ला देता है वह उसे ग्रहण करता है, वह किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता : जो उसके पास आता है उसे वह आसक्ति और विकर्षण के बिना ग्रहण करता है; जो कुछ उससे चला जाता है उसके लिए बिना प्रलाप या शोक किये या बिना किसी हानि के बोध के उसे संसार-चक्र में जाने देता है। उसका हृदय और अंतःकरण पूर्णतः उसके वश में होते हैं; वे समस्त प्रतिक्रिया या आवेश से मुक्त होते हैं, वे बाह्य विषयों के स्पर्श की कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं करते। वस्तुतः, उसका कर्म केवल एक शारीरिक कर्ममात्र होता है, शारीरं केवलं कर्म; क्योंकि बाकी सब कुछ तो ऊपर से आता है, मानव-स्तर पर उत्पन्न नहीं होता, भगवान् पुरुषोत्तम के संकल्प, ज्ञान और आनन्द का प्रतिबिंब-मात्र होता है। इसलिए वह कर्म और उसके उद्देश्यों पर बल देकर भी अपने मन और हृदय में उनमें से वे कोई भी प्रतिक्रियाएँ नहीं उत्पन्न करता जिन्हें हम आवेश और पाप की संज्ञा देते हैं। क्योंकि पाप बिल्कुल भी बाह्य कृत्य में नहीं होता, अपितु व्यक्तिगत इच्छा, मन तथा हृदय की अशुद्ध प्रतिक्रिया में होता है जो उस कर्म के साथ संलग्न रहती है अथवा उस कर्म को कराती है; नैयक्तिक आध्यात्मिक मनुष्य तो सदा ही शुद्ध, अपापविद्धं, होता है और जो कुछ भी वह करता है उस सब को भी स्वयं अपनी वह सहज अपरिहार्य शुद्धता प्रदान कर देता है। यह आध्यात्मिक नैर्व्यक्तित्व दिव्य कर्मी का तीसरा लक्षण है। वस्तुतः, किसी अमुक प्रकार की महानता तथा विशालता को प्राप्त सभी मनुष्य एक ऐसी नैयक्तिक शक्ति या प्रेम या संकल्प और ज्ञान के विषय में सचेतन होते हैं जो उनके द्वारा कार्य कर रहे होते हैं, परंतु वे अपने मानव-व्यक्तित्व की अहंभावापन्न प्रतिक्रियाओं से, जो कभी-कभी अत्यंत प्रचंड होती हैं, मुक्त नहीं हो पाते। परन्तु मुक्त पुरुष इस मुक्ति को प्राप्त करता है; क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व को नैयक्तिक पुरुष में निक्षेप कर दिया होता है, जहाँ उसका वह व्यक्तित्व उसका अपना नहीं रह जाता, अपितु उन दिव्य पुरुष, पुरुषोत्तम, द्वारा हाथों में ले लिया जाता है जो सभी सीमित गुणों को अनन्त और मुक्त रूप से उपयोग करते हैं और किसी के द्वारा बद्ध नहीं होते। मुक्त पुरुष आत्मा बन जाता है और प्रकृति के गुणों का पुंज नहीं बना रहता; और प्रकृति के कर्म के लिए उसके व्यक्तित्व का जो कुछ आभास बाकी रह जाता है वह एक ऐसी चीज होती है जो बंधनमुक्त, उदार, नमनीय और विश्वव्यापक होती है, यह अनन्त के लिए एक मुक्त पात्र होता है, पुरुषोत्तम का एक जीवंत आवरण हो जाता है।
दिव्य कर्मी के सारे कर्म निर्वैयक्तिक होते हैं। उसे एक पृथक् व्यक्तित्व का बोध नहीं होता कि वह स्वयं कोई कर्म कर रहा है। यह तीसरी चीज है। ऐसे व्यक्ति में एक तो अहं नहीं होता, दूसरे कामना नहीं होती और तीसरे वह निर्वैयक्तिक होता है। इसलिए ऐसा दिव्य कर्मी भले कितने भी घोर रूप से कर्म क्यों न कर ले, उस पर उन कर्मों का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता। यदि हम इस सारी चीज को सतही दृष्टिकोण से देखें - जैसे कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को, दिव्य कर्मी के लक्षणों को - तो हम पाएँगे कि वास्तव में तो ये प्रारंभिक चीजें प्रास करना भी इतना मुश्किल है कि व्यक्ति इनसे आगे की तो सोच भी नहीं सकता। परन्तु हमें यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि ये सभी चीजें और अवस्थाएँ अपने पूर्ण और परिशुद्ध रूप में कभी प्राप्त नहीं होतीं। अपने पूर्ण रूप में ये सभी होने के लिए तो पूर्ण सिद्धि अर्थात् सभी चीजों के रूपांतर होने की आवश्यकता है। हमारे निश्चेतन और अवचेतन आदि निम्न भागों के पूर्ण रूपांतरण के बिना तो इनका प्रभाव सदा ही हमारी सभी स्थितियों को तथा हमारी सभी चीजों को दूषित करता रहेगा और उन्हें नीचे खींचता रहेगा। स्थितप्रज्ञ आदि तो केवल किन्हीं स्थिति विशेष का वर्णन करने के लिए हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी आत्मपरक (subjective) चेतना में तो प्राप्त कर सकता है, परंतु वास्तव में जब तक हमारे निम्न भागों द्वारा उच्चतर भागों में प्रवेश करने की और क्रिया करने की आशंका बनी रहेगी, और जब तक इन भागों को पूरी तरह रूपांतरित नहीं किया जाता, तब तक व्यक्ति का संतुलन सदा ही संदिग्ध बना रहेगा और उसे कभी भी बिगाड़ा जा सकता है। यदि ऐसा न होता तो अब तक तो सहज रूप से सभी कुछ सिद्ध किया जा चुका होता। अतः योग की जिन स्थितियों का हम वर्णन पाते हैं, वे स्थितियाँ वास्तव में केवल एक निश्चित सीमा तक ही रह सकती हैं। हालाँकि, वे एक बहुत गहरी सीमा तक हो सकती हैं, परन्तु पूर्ण नहीं हो सकतीं। जब तक पूर्ण रूप से रूपांतर नहीं हो जाता तब तक वास्तव में कोई भी चीज पूर्ण नहीं हो सकती। गीता यही बताएगी कि कैसे व्यक्ति इस तक पहुँच सकता है। वह कहती है कि जब व्यक्ति यज्ञ के रूप में कर्म करना आरंभ करेगा, तब उसका ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। ज्ञान बढ़ेगा तो कर्म उसके प्रकाश में बेहतर हो जाएगा। और जब कर्म और अधिक यज्ञमय होगा तो ज्ञान और अधिक बढ़ेगा। इस प्रकार ज्ञान और कर्म एक-दूसरे को आगे बढ़ाते चलेंगे जैसे कि दाएँ और बाएँ पैर के तालमेल से व्यक्ति आगे बढ़ता है। वैसे ही ज्ञान और कर्म एक-दूसरे को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर एक सीमा पर पहुँचने पर भक्ति का समावेश हो जाता है। भक्ति कर्म का आधार और ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। जब ज्ञान एक सीमा तक पहुँच जाता है तब भक्ति उदय होती है। कर्म का सच्चा आधार भक्ति है, उसके बिना कर्म में वह सार, वह दिव्यता, वह मुक्ति नहीं आ सकती। ज्ञान के द्वारा कर्म एक सीमा तक ही जा सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है। हमें गीता के उपदेश व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने पर कुछ-कुछ समझ में आते हैं। अन्यथा आरंभ में ही भगवान् जब निष्काम कर्म करने का उपदेश देते हैं तब कोई भी व्यक्ति असमंजस में पड़ जाएगा कि आखिर निष्काम कर्म वास्तव में संभव ही कैसे हो सकते हैं? इसके विषय में श्रीअरविन्द ने अपनी पुस्तक 'योग-समन्वय' में कहा है कि व्यक्ति निष्काम कर्म की ओर चलना शुरू तो कर सकता है परन्तु वह एकाएक ही पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक अहं है तब तक यह संभव नहीं है क्योंकि व्यक्ति का सबसे पहले तो स्वयं कर्म से ही लगाव रहता है। वह उससे आगे जा ही नहीं पाएगा। और अहं सहज ही नष्ट नहीं हो सकता। केवल अपने गहरे भागों में ही व्यक्ति इससे कुछ मुक्ति का अनुभव कर सकता है परंतु जब तक अवचेतन और निश्चेतन भाग मौजूद हैं, जब तक भौतिक शरीर है तब तक पूर्ण रूप से अहंमुक्त चेतना संभव नहीं है। और यदि समाधि अवस्था में उस पूर्ण अहंमुक्त चेतना का आस्वादन हो भी जाए तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि निर्विकल्प समाधि की अवस्था में भौतिक शरीर को बनाए रखना अधिक संभव नहीं हो पाता और इक्कीस दिनों के बाद वह नष्ट हो जाता है।
प्रश्न : जैसा कि दिव्य कर्मी के पहले दो लक्षण बताए गए हैं, उनके अनुसार इसका अर्थ क्या यह निकलता है कि उस चेतना में रहने पर इच्छाएँ और कामनाएँ झड़ जाती हैं?
उत्तर : यह कोई इतनी सीधी-सरल बात नहीं है कि इसे किसी एक मानसिक सूत्र में बाँध दिया जाए। व्यक्ति को अहं-मुक्त चेतना का अनुभव तो हो सकता है परन्तु वास्तव में ये चीजें यों ही जाने वाली नहीं हैं, और यहाँ तक कि इनका समाप्त होना सर्वथा उचित भी नहीं है। वास्तव में हमें करना यह चाहिए कि अपनी कामनाओं और अहं को श्रीमाताजी को समर्पित कर दें और फिर वे उनका जैसा चाहें वैसा उपयोग करें। क्योंकि भगवान् की ओर चलना इतना आसान नहीं है। अधिकांश धार्मिक पुस्तकों में सामान्यतः जो शिक्षा दी जाती है उनमें ये ही तो खामियाँ हैं जो कहती हैं कि अहं और कामना आदि को मार डालना चाहिए। परन्तु वास्तव में हम यह नहीं जानते कि हमारी कौन-सी कामना भगवान् की अभिव्यक्ति के लिए कहाँ उपयुक्त सिद्ध हो सकती है और भगवान् की अभिव्यक्ति के अंदर अहं की भी उपयोगिता कहाँ हो सकती है। यह कोई ऐसी सरल बात नहीं है कि कामना समाप्त हो गई तो व्यक्ति लक्ष्य तक पहुँच गया। व्यक्ति का जैसा संपूर्ण गठन होता है उसी के अनुसार वह भगवान् की ओर चलता है और इस यात्रा में कौन-सी कामना आवश्यक है और कौन-सी नहीं, और कितनी कामना इस दौरान मिट जाएगी और कितनी नहीं, या फिर कामना रूपांतर की प्रक्रिया में सहायक है या नहीं, इन सब को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। ये सब सूत्र तो केवल मोटे रूप से समझाने के लिए होते हैं, जबकि वास्तव में पूरी प्रक्रिया कोई इतनी नियत-निर्धारित नहीं होती। हम इसके लिए कितने ही भक्तों के जीवन के उदाहरण देख लें पर उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि ऐसा कोई सीधा-सरल सूत्र देखने को मिलता हो। हाँ, यह हो सकता है कि जब व्यक्ति भगवान् को, या अपने गुरु को या श्रीमाताजी को जितना ही समर्पित होता जाता है उसकी इच्छाएँ, कामनाएँ जितनी आवश्यक होंगी उन सबको वे स्वयं ही काम में लेंगे। जैसे कि श्रीरामकृष्ण जी कहते थे कि 'मेरी कामनाएँ-इच्छाएँ तो वैसी ही हो गई हैं जैसे कि कोई जल चुकी रस्सी, क्योंकि अब वे कामना आदि आत्मा को बाँध नहीं सकतीं।' परन्तु कुछ लोग जो कामना और अहं आदि से मुक्ति के बाहरी लक्षणों पर ही बल देते हैं वे इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि वे उनसे मुक्त हो चुके हैं और इससे तो वे और अधिक मिथ्यात्व में गिर जाते हैं। इसलिए अधिक अच्छा है कि व्यक्ति सहज रूप से रहे। क्योंकि हमारे किन्हीं भी बाहरी मानदण्डों के आधार पर यह पता ही नहीं चल सकता कि कामनाएँ कौनसी हैं और कौनसी नहीं। और जब व्यक्ति श्रीमाताजी के प्रति समर्पित होता है तब उसकी सारी कामनाएँ संकल्प में परिवर्तित हो जाती हैं। परंतु संकल्प में और कामना में अन्तर करना बहुत ही कठिन है। बाह्य दृष्टिकोण से तो श्रीमाताजी भी सभी मानवीय क्रियाकलाप करती थीं। वे भोजन भी करती थीं, लोगों से कार्य-व्यवहार भी करती थीं, आश्रम की सार-संभाल का कार्य भी करती थीं। और जिसके साथ जैसा आवश्यक था वैसा व्यवहार भी करती थीं। एक बार उन्हें किसी पर बड़ा क्रोध आया। बाद में उन्होंने सोचा कि क्या अभी तक वे इसी स्थिति में हैं कि उन पर क्रोध हावी हो सकता है। परंतु फिर तुरंत ही भीतर से उन्हें इसका उत्तर प्राप्त हुआ कि संसार में वे अपनी व्यक्तिगत पूर्णता के लिए कार्य नहीं कर रहीं। उनके द्वारा परम् प्रभु वैश्विक दृष्टिकोण से जहाँ जो आवश्यक होता है उस प्रकार की क्रिया करवा लेते हैं। इसलिए भगवान् के काम के लिए जो भाव आवश्यक होगा वही उनके अन्दर स्वतः ही आ जाएगा और अभिव्यक्त हो जाएगा। इसलिए किसी एक सूत्र में बँध कर यह कहना कि मैं कामना से मुक्त हूँ, अहं से मुक्त हूँ, ये सब अनावश्यक बातें हैं। वास्तव में तो सारी चीज का निर्धारण ऊपर से जगदम्बा करती हैं, इसलिए हम अपने मानवीय मानदंडों के आधार पर कुछ नहीं कह सकते हैं। जो व्यक्ति व्यवहार में इसे जीता है उसे तो इन बातों का भान होता है। योग-साधना के अंदर स्थितप्रज्ञ आदि जिन स्थितियों का वर्णन आता है वे तो केवल समझाने मात्र के लिये हैं। गीता में भी ये बातें अर्जुन की बुद्धि में प्रकाश लाने के लिए उसे समझाई गई हैं। परंतु ये तो केवल आरंभ में ही बताई गई हैं। गहरी चीजें तो केवल बाद में ही उसके सामने प्रकट की गई हैं। इसलिए इन सबकी तो कर करने का प्रयास करना तो मूढ़ता है। व्यक्ति के अचेतन और निश्चेतन भाग ऐसे नहीं हैं जिन्हें कि किन्हीं भी मानसिक सूत्रों से नियंत्रित और संयमित किया जा सके।
प्रश्न : मेरा प्रश्न यह नहीं था कि अहं और कामनाओं से कैसे मुक्त होना है। मेरा प्रश्न तो यह था कि क्या ऐसा नहीं है कि जब हम आत्म-चेतना में रहते हैं तो इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं?
उत्तर : यह ऐसी चीज नहीं है। क्या श्रीमाताजी आत्म-चेतना में निवास नहीं कर रहीं थीं? तब फिर उन्हें क्रोध आदि कैसे आते थे? हम किन बाहरी मापदंडों के आधार पर उनकी क्रियाओं का आकलन करें? आखिर आत्म-चेतना कहते किसे हैं? इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति ध्यान की अवस्था में रहकर सतही चेतना से अपने को अलग कर लेता है। ऐसी बात नहीं है। घोर कर्म में रत रहने पर भी आत्म-चेतना हो सकती है और वहीं गहन ध्यान की अवस्था में रहते हुए, शांत-चित्त रहते हुए भी आवश्यक नहीं है कि आत्म-चेतना हो। हो सकता है कि व्यक्ति किसी मानसिक संरचना में या फिर अपने ही किसी व्यक्तिगत मानसिक जगत् में फँसा हुआ हो। इसलिए यह हमें बहुत ही स्पष्ट कर लेना होगा कि आत्म-चेतना कोई बँधी-बँधाई चीज नहीं है। यह तो किसी चीज को समझाने के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है। यों तो हमारे अन्दर और हमारी हर चीज के अन्दर आत्मा विद्यमान है। आत्मा तो सभी कुछ है तो फिर आत्म-चेतना जैसी कोई अलग चीज कहाँ से आ जाएगी। आत्मा, प्रकृति आदि शब्द तो केवल मानसिक रूप से समझाने के लिए हैं, व्यावहारिक रूप से चीजें बहुत अधिक जटिल हैं। जब तक हमें स्वयं जीवंत अनुभव नहीं होगा और हम इन मानसिक विचारों में ही रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते। वास्तव में तो कुछ भी पता नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है। यह तो वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसे कुछ-कुछ पथ-निर्देश दिये जाते हैं। ये सब उसी तरीके को चीजें हैं। इसीलिए तो सभी लोग बार-बार कहते हैं कि बिना जीये इन चीजों को समझा नहीं जा सकता। वास्तव में कोई नियत-निर्धारित भेद नहीं हैं कि यह यौगिक चेतना है और यह उससे विपरीत है, या फिर यह आत्म-चेतना है और यह नहीं है। इन सब विषयों में भेद इतना सूक्ष्म है कि वह मन की पकड़ में नहीं आता। ये सब चीजें तो केवल अनुभव से ही समझ में आ सकती हैं। जैसे हम केवल समझने-समझाने के लिए ही मन, प्राण और शरीर आदि विभिन्न हिस्सों में भेद करते हैं जबकि श्रीअरविन्द कहते हैं कि वास्तव में तो उनमें ऐसा कोई स्पष्ट अलगाव नहीं है। यह तो ऊपर से नीचे तक सारी एक अटूट श्रृंखला है। केवल मानसिक रूप से देखने और समझने के लिए ही भेद किया जाता है जबकि वास्तव में तो इनमें कोई अलगाव नहीं है। इसीलिये मानसिक रूप से ये चीजें समझ में नहीं आ सकतीं क्योंकि इसमें मानसिक संरचनाओं का निर्माण हो जाता है जो कि सत्य को छिपा देती हैं। मन की समस्या यह है कि पहले तो वह सत्य के किसी एक अंश को पकड़ता है और उसे भी बड़े ही अपूर्ण रूप से समझता है। और फिर उसी को पूर्ण सत्य मानने पर आग्रह करता है और फिर उसे दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है। और इससे वह चीज मिथ्या हो जाती है। जबकि वास्तविक बात तो बहुत गहरी है।
इच्छाएँ, कामनाएँ आदि खत्म होना अपने-आप में उद्देश्य नहीं बल्कि परिणाम है। इच्छाएँ, कामनाएँ तो इसलिए समाप्त होती हैं कि व्यक्ति को ऐसी श्रेष्ठ चीजें प्राप्त हो रही होती हैं और इतनी अधिक प्राप्त हो रही होती हैं कि वह दूसरी किन्हीं चीजों की इच्छा कर ही नहीं सकता। और यह सोचना कि मुझे इच्छा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इच्छा करना तो पाप हो जाएगा, इस तरीके से कभी भी इच्छाएँ वश में नहीं हो सकतीं। इच्छाएँ-कामनाएँ तो तभी समाप्त होती हैं जब हमें परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और इसके बाद भी जिन हिस्सों में वह प्रकाश अभी नहीं पहुँचा होता उनमें छोटी-छोटी इच्छाएँ, कामनाएँ उठती रहती हैं। अच्छे-अच्छे महात्माओं तक से छोटी-छोटी इच्छाएँ नहीं छूट पार्टी। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति के कार्य करने का तरीका बहुत ही जटिल है। सच्ची बात तो एक ही है कि किसी भी तरीके से हम अपने-आप को भगवान् की ओर, श्रीमाताजी की ओर मोड़ दें, और फिर जो होना हो सो हो। अन्यथा तो यह प्रयास करते रहना कि मैं अपनी इच्छाओं को वश में कर के निष्काम हो जाऊँ, तो इसमें हम कितना भी समय व्यर्थ क्यों न बिता दें, पर ऐसा होना संभव नहीं है। और वहीं यदि व्यक्ति श्रीमाताजी की सेवा में लग जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि वह कब निष्काम हो गया। जिसको निष्काम होने और साधना करने में कोई रुचि नहीं है वही वास्तव में निष्काम हो सकता है, परंतु जिसे निष्काम होने की चिंता है वह कभी भी निष्काम नहीं हो सकता और न ही कभी उसकी साधना ही हो सकती है, वह तो केवल अपने-आप को धोखा भले ही दे सकता है। अधिकांश लोगों की तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं होती कि वे किसी छोटे से अनुभव को भी पचा सकें। अतः भगवान् बड़े कृपालु हैं कि अनधिकारी और अयोग्य व्यक्ति को इस तरीके के कोई अनुभव देते ही नहीं। व्यक्ति को कदम-कदम पर यह पता होना चाहिए कि वह अभी कितना अपरिपक्व है। इसलिए कामनाएँ, इच्छाएँ आदि तो ऐसी उपयोगी चीजें हैं जो व्यक्ति को कम-से-कम धरातल पर तो बनाए रखती हैं। अन्यथा तो वह इतना आत्म-संतुष्ट और अपने-आप के विषय में इतने मिथ्याभिमानों से भर जाता कि उससे छूट पाना तो संभव ही नहीं होता, हालाँकि बिना किन्हीं अनुभवों के भी पहले से ही वह मिथ्याभिमान से खूब भरा हुआ होता है। सामान्यतः जब व्यक्ति कहता कि वह निष्काम हो चुका, निस्पृह हो चुका है, सबको समान दृष्टि से देखता है, तो ये सब बिल्कुल मिथ्या बातें होती हैं क्योंकि वह अपने मिथ्याभिमान से भरा होता है। अतः श्रीमाताजी बड़ी ही दयालु हैं जो साधना और योग के मिथ्याभिमानों से हमारी रक्षा करती हैं।
यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।। २२।।
२२. जो मनुष्य (भगवदिच्छा से) जो कुछ भी उसे प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है, (हर्ष-शोक, मान-अपमान, जय-पराजय, पाप-पुण्य आदि) समस्त द्वन्द्वों से अतीत हो गया है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सफलता और विफलता में सम रहता है वह कर्म करता हुआ भी बद्ध नहीं होता है।
इस ज्ञान, निष्कामता और नैयक्तिकता का परिणाम है आत्मा और प्रकृति में पूर्ण समत्व। समत्व दिव्य कर्मी का चौथा लक्षण है। गीता कहती है कि वह 'द्वन्द्वातीत' हो जाता है। हमने देखा है कि वह सफलता और विफलता, जय और पराजय को अविचल भाव से और समदृष्टि से देखता है; अपितु ये ही नहीं सभी द्वन्द्व उसमें अतिक्रम कर दिये जाते हैं और समस्वर बना दिये जाते हैं। जिन बाह्य लक्षणों से मनुष्य जगत् की घटनाओं के प्रति अपनी मनोवृत्ति का रुख निश्चित करते हैं वे उसकी दृष्टि में गौण और यांत्रिक होते हैं। वह उनकी उपेक्षा नहीं करता, पर उनसे परे (ऊपर) रहता है। शुभ और अशुभ, जो कि कामना के वशीभूत मनुष्य के लिए अत्यावश्यक चीज है, परंतु निष्काम आत्मवान् पुरुष के लिए ये दोनों समान ही सहर्ष स्वीकार्य हैं, क्योंकि इन दोनों के सम्मिश्रण से ही शाश्वत शुभ के विकसनशील रूप निर्मित होते हैं। उसे पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए तो प्रकृति के कुरुक्षेत्र अर्थात् धर्मक्षेत्र में, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस कर्मक्षेत्र में जो विकसनशील धर्म का क्षेत्र है, सभी कुछ ही भागवत् विजय की ओर गति कर रहा है, और युद्ध के प्रत्येक मोड़ का नक्शा युद्ध के अधिनायक, कर्मों के स्वामी, धर्म के नेता की पूर्वदृष्टि द्वारा पहले ही खींचकर तैयार किया जा चुका है। मनुष्यों से मिलनेवाला मान या अपमान तथा उनकी निन्दा या स्तुति उसे विचलित नहीं कर सकती हैं; क्योंकि उसके पास एक श्रेष्ठतर स्पष्ट द्रष्टा निर्णायक होता है और उसके कार्य का एक अलग मापदण्ड होता है, और उसका ध्येय या प्रेरक-भाव सांसारिक पुरस्कार पर निर्भरता को जरा भी स्वीकार नहीं करता।
उसे किसी भी निजी हेतुओं की पूर्ति नहीं करनी होती, कोई निजी राग-द्वेषों की तुष्टि नहीं करनी होती, कर्म के संबंध में वह ऐसा कोई कठोर रूप से निर्धारित मानदण्ड नहीं रखता जो मनुष्यजाति की उन्नति की ओर बढ़ती हुई सुनम्य अग्रगति के विरुद्ध अपनी पत्थर की लकीर को अर्थात् रूढ़ नियमों को खड़ा कर दे, या फिर अनन्त की पुकार की अवज्ञा करता हुआ उसके विरुद्ध खड़ा हो जाए। उसके कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं जिन्हें उसे जीतना या मारना हो, अपितु वह केवल ऐसे लोगों को देखता है जिन्हें परिस्थिति ने और वस्तुओं में निहित संकल्प ने उसके विरुद्ध लाकर इसलिए खड़ा कर दिया है कि वे अपने प्रतिरोध के द्वारा भवितव्यता की गति में सहयोग करें। इन लोगों के विरुद्ध उसके मन में कोई प्रचण्ड क्रोध या घृणा नहीं हो सकती क्योंकि दिव्य प्रकृति के लिये क्रोध और घृणा विजातीय चीजें हैं। असुर की अपने विरोधी को चूर-चूर करने और उसका वध कर डालने की इच्छा, राक्षस की संहार करने की निर्दयतापूर्ण लिप्सा का मुक्त पुरुष की स्थिरता, शान्ति और उसकी सर्वालिंगनकारी सहानुभूति और समझ में होना असम्भव है। उसमें किसी को क्षति पहुँचाने की इच्छा नहीं होती, अपितु इसके विपरीत, विश्वव्यापी मैत्री और करुणा होती है, मैत्रः करुण एव च : परंतु यह करुणा उस दिव्य आत्मा की करुणा है जो मनुष्यों को उच्चासीन होकर देखता है, सब जीवों को अपने अन्दर प्रेम से ग्रहण करता है, यह कोई हृदय, स्नायुओं और देह या भावनाओं का दुर्बल कंपन या संकुचन नहीं है जैसी कि सामान्य मानव रूप में दया होती है। न ही वह शरीर के जीवन को ही परम् महत्त्व प्रदान करता है, अपितु इसके परे आत्मा के जीवन पर दृष्टि रखता है और शरीर को केवल एक उपकरण समझता है। वह सहसा ही संग्राम और संहार में प्रवृत्त न होगा, पर यदि धर्म के प्रवाह में युद्ध समक्ष आ पड़े तो वह उसे व्यापक समता के साथ और जिन लोगों की सत्ता और प्रभुत्व के भोग को उसे चूर्ण करना है और जिनके विजयी जीवन के उल्लास को उसे नष्ट करना है उनके प्रति सहानुभूति और पूर्ण सद्भाव के साथ वह उसे स्वीकार करेगा।
क्योंकि सबमें वह दो चीजें देखता है, एक है सभी में समान रूप से वास करते भगवान् को, और दूसरी उनकी नानाविध अभिव्यक्ति को जो अपनी अनित्य परिस्थितियों में ही असमान या विषम है। पशु में, मनुष्य में, कुक्कुर में. अशुचि जाति-बहिष्कृत में, विद्वान् में, ज्ञानी और गुणी ब्राह्मण में, संत में और पापी में, उदासीन में, प्रेमी में और विरोधी में, उनमें जो उसे प्यार करते और उसका उपकार करते हैं और उनमें जो उससे घृणा करते और उसे पीड़ा पहुँचाते हैं, (उन सब में) वह अपने-आपको देखता है, ईश्वर को देखता है और उसके हृदय में सबके लिए एक समान ही करुणा और दिव्य प्रीति होती है। परिस्थितियाँ उसके बाह्य आलिंगन या बाह्य संघर्ष को निर्धारित कर सकती हैं. परंतु वे कभी भी उसकी समदृष्टि को, उसके खुले हृदय को और सभी के प्रति आंतरिक आलिंगन के भाव को प्रभावित नहीं कर सकतीं। और उसके सभी कर्मों में आत्मा का एक ही विधान, अर्थात् पूर्ण समत्व होगा और वही सिद्धांत कर्म का होगा, उसके अंदर भगवान् की ओर क्रमशः अग्रसर होती हुई मानव जाति की आवश्यकता के लिए भगवान् का संकल्प क्रियाशील होगा।
यह तो एक स्पष्ट बात है कि जब व्यक्ति यह देखने में सक्षम हो जाता है कि किस प्रकार यह सारा संसार भगवान् की ओर चल रहा है, और वह इसके सारे उतार-चढ़ावों को और इसकी सारी व्यवस्था को समझ जाता है तब उसमें समता आ जाती है। व्यक्ति की सोच-समझ, उसका दृष्टिकोण, उसके सिद्धांत आदि बहुत ही सीमित और संकुचित होते हैं इसीलिए उसे जीवन में वस्तुएँ अच्छी-बुरी, सही-गलत आदि लगती हैं। परन्तु ईश्वर के दृष्टिकोण में हर चीज का अपना एक उचित स्थान है। जब मनुष्य ईश्वर के दृष्टिकोण को कुछ-कुछ समझने लगता है तो उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता जाता है, निजी पसन्द-नापसन्द आदि पर अतिशय आग्रह कम होने लगता है और समता आ जाती है। जैसे कि यदि हम किसी चित्रकार को कोई चित्र बनाते हुए देखें तो बहुत ही प्राथमिक स्तर पर हमें पता ही नहीं होता कि वह क्या बनाना चाह रहा है और उसके द्वारा काम में लिए जाने वाले रंगों आदि को हम उस चित्र की आवश्यकता के आधार पर न देख कर अपनी ही पसन्द-नापसन्द
२३. जब मनुष्य मुक्त हो जाता है, आसक्ति से रहित हो जाता है, जिसके मन, हृदय और आत्मा आत्मज्ञान में दृढ़प्रतिष्ठित हो गये हैं और जो यज्ञ के रूप में कर्म करता है तो उसका सम्पूर्ण कर्म विलीन हो जाता है।
ज्ञान से कामना और उसकी प्रथम संतान, पाप, का ध्वंस होता है। मुक्त पुरुष कर्मों को यज्ञरूप से कर पाता है, क्योंकि उसके मन, हृदय और आत्मा के आत्मज्ञान में दृढ़प्रतिष्ठ होने के कारण वह आसक्ति से मुक्त होता है, गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । उसके सारे कर्म होने के साथ ही सर्वथा लय को प्राप्त हो जाते हैं, कहा जा सकता है कि वे ब्रह्म की सत्ता में विलीन हो जाते हैं, प्रविलीयते; बाह्य पात्ररूप जो कर्त्ता होता है उसकी अंतरात्मा पर उन कर्मों का कोई प्रतिगामी परिणाम नहीं होता। भगवान् ही उस कर्म को अपनी प्रकृति के द्वारा करते हैं, वे मानव-उपकरण के निजी नहीं रह जाते... भगवान् ही संपूर्ण कर्म का प्रवर्तन, प्रेरण और निर्धारण करते हैं; मानव-आत्मा ब्रह्म में नैयक्तिक भाव को प्राप्त होकर उनकी शक्ति का विशुद्ध और शांत माध्यम बनती है; यही शक्ति प्रकृति में दिव्य कर्म संपादन करती है। केवल इसी प्रकार के मुक्त पुरुष के कर्म होते हैं, मुक्तस्य कर्म; क्योंकि किसी भी चीज में मुक्त पुरुष किसी व्यक्तिगत प्रवृत्ति से कर्म नहीं करता; ऐसे होते हैं सिद्ध कर्मयोगी के कर्म। ये कर्म एक मुक्त आत्मा से उदित होते हैं और उसमें कोई विकार या संस्कार उत्पन्न किये बिना ही विलीन हो जाते हैं, जैसे, अक्षर अगाध चित्-समुद्र में लहरें ऊपर उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं।
परन्तु आत्मानुशासन या साधना के किन व्यावहारिक क्रमों या उपायों से हम इस सिद्धि तक पहुँच सकते हैं?
समस्त अहंमूलक क्रिया और उसके आधार, अहंमय चेतना, का निर्मूलन करना स्पष्टतः ही हमारी अभीष्ट सिद्धि का उपाय है। और, क्योंकि कर्मयोग के पथ में कर्म ही वह सबसे पहली ग्रंथि होती है जिसे हमें खोलना होता है, हमें इसे वहीं से खोलने का प्रयत्न करना होगा, अर्थात् कामना और अहंभाव में, जहाँ यह केंद्रीय (प्रधान) रूप से बँधी हुई है; क्योंकि, अन्यथा हम केवल कुछ बिखरे धागे ही काटेंगे न कि अपने बंधन के मर्मस्थल को। इस अज्ञानमय एवं विभक्त प्रकृति के प्रति हमारी अधीनता की ये ही दो ग्रंथियाँ हैं कामना और अहंभाव। और इन दो में से कामना का मूल निवासस्थान या जन्मस्थान है भावावेगों, संवेदनों और अन्ध-वृत्तियों में, और वहीं से यह विचारों और इच्छाशक्ति पर अपना प्रभाव डालती है। निस्संदेह अहंभाव इन चेष्टाओं में रहता ही है, परंतु साथ ही वह चिन्तनात्मक मन और उसकी इच्छाशक्ति में भी अपनी गहरी जड़ें फैलाता है और वहीं वह पूर्णतः आत्म-सचेतन भी होता है। ग्रसित कर देने वाली जगद्व्यापिनी अविद्या की ये ही युगल अन्धकारमय शक्तियाँ हैं जिन्हें हमें प्रकाश में लाना और बहिष्कृत करना होगा।
कर्म के क्षेत्र में कामना अनेक रूप धारण करती है, किन्तु उन सब में सबसे अधिक प्रबल रूप है अपने कर्मों के फल के लिये प्राणमय पुरुष की लालसा या उत्कण्ठा। जिस फल की हम लालसा करते हैं वह आन्तरिक सुख रूपी पुरस्कार हो सकता है; वह किसी मनोनीत विचार या किसी प्रिय संकल्प की पूर्ति या अहंकारमय भावों की तृप्ति, या फिर अपनी उच्चतम आशाओं और महत्त्वाकांक्षाओं की सफलता का गौरवरूपी पुरस्कार हो सकता है। अथवा वह एक बाह्य पारितोषिक हो सकता है, एक सर्वथा द्रव्यात्मक प्रतिफल हो सकता है, जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा, विजय, सौभाग्य अथवा प्राणिक या शारीरिक कामना की किसी और प्रकार की तृप्ति। परन्तु हैं ये सब समान रूप से ऐसे फंदे जिनके द्वारा अहंभाव हमें बाँध लेता है। सदा ही ये सुख-सन्तोष हमें स्वामित्व के बोध से और स्वतन्त्रता के विचार से भ्रमित करते हैं अथवा छलते हैं, जबकि वास्तव में अन्ध 'कामना' की कोई स्थूल या सूक्ष्म, भली या बुरी मूर्ति ही – जो जगत् को प्रचालित करती है, - हमें जोतती है और चलाती है अथवा हम पर सवार होती और हमें कोड़े लगाती है। इसलिये गीता द्वारा प्रतिपादित कर्म का जो सबसे पहला नियम है वह है, निष्काम कर्म, फल की किसी भी प्रकार की कामना के बिना कर्तव्य कर्म करना।
दिव्य कर्मी के लक्षणों का वर्णन सुनकर, कि वह हमेशा हर परिस्थिति में सम रहता है तथा कामनाओं एवं अहंभाव से मुक्त होता है, प्रश्न यह उठता है कि ये सब गुण प्राप्त कैसे किए जाएँ? दिव्य कर्मी के जो लक्षण बताए गए हैं कि - वह आसक्ति से मुक्त होता है, उसके सारे कर्म भगवान् के द्वारा किए जाते हैं आदि-आदि - ये सब पहचान के लिए तो ठीक हैं पर पहचान भी बाहरी रूप से नहीं हो सकती क्योंकि ये सब तो आन्तरिक लक्षण हैं। इसलिये सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि व्यक्ति इन सब गुणों को प्राप्त कैसे करे?
श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि हमारी अधीनता की जड़ें अहंभाव और कामना में हैं। कामना का सबसे पहला, बाहरी और सदा ही बना रहने वाला प्रारूप यह है कि हम जो कोई भी कर्म करते हैं, उससे हमेशा ही कोई न कोई फल की - चाहे वह बाहरी हो या आन्तरिक, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, भौतिक हो या प्राणिक, सूक्ष्म हो या स्थूल- आशा रखते हैं और हमेशा ही किसी-न-किसी संतोष की खोज में रहते हैं। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक हमारे कर्म इससे प्रभावित होते रहेंगे। हम अपने प्रत्येक कर्म को इसी तराजू पर तोलते रहेंगे कि कौन-सा कर्म हमें हमारी कामना के अनुसार संतोष और सफलता प्रदान करेगा और कौन-सा नहीं। इस प्रकार हम कभी भी सही और सच्चे भाव से कर्म नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जब तक हम अपने इस सीमित दृष्टिकोण से कर्म को देखेंगे तब तक हम पूर्वाग्रहों से, अपने-पराये, सही-गलत आदि द्वंद्वों से बँधे रहेंगे और सही निर्णय नहीं कर सकेंगे। अतः इसके लिये जो पहला नियम बताया गया है वह यह है कि, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'। परन्तु बिना कर्मफल की कामना के तो हम कर्म कर ही नहीं सकते इसलिए इससे भी यह समस्या हल होने वाली नहीं है क्योंकि पहले तो हम स्वयं को ही धोखा देंगे और दूसरे यह काम हमारे वश में नहीं है, हम प्रयास कर के भी इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि कामना बहुत शक्तिशाली और जिद्दी प्रकृति की है। और फिर, जैसा कि श्रीअरविन्द कहते हैं कि यह काम टुकड़ों में होने वाला भी नहीं है। समग्र पूर्णता में ही यह संसिद्ध हो सकता है।
देखने में तो यह नियम सीधा-सादा दिखता है, पर फिर भी इसे किसी प्रकार की पूर्ण सच्चाई और मोक्षप्रद समग्रता के साथ निभाना कितना कठिन है! हमारे कर्म के अधिक बड़े भाग में यदि हम इस सिद्धान्त का प्रयोग करते भी हैं तो बहुत कम, और तब भी प्रायः कामना के सामान्य नियम को एक प्रकार से सन्तुलित करने और इस क्रूर आवेग की अतिशयित क्रिया को कम करने के लिये ही करते हैं। अधिक-से-अधिक हम इतने भर से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं यदि हम अपने अहंभाव को संयत और संशोधित कर लें जो हमारी नैतिक भावना को बहुत अधिक ठेस पहुँचाने वाला और दूसरों को अत्यन्त निर्दयतापूर्वक पीड़ा पहुँचाने वाला न रहे। और, हमारे इस आंशिक आत्मानुशासन को हम अनेक नाम और रूप दे देते हैं; अभ्यास के द्वारा हम कर्तव्य-बोध, सिद्धान्त के प्रति दृढ़-निष्ठा, वैराग्यपूर्ण सहिष्णुता या धार्मिक समर्पण और ईश्वरेच्छा के प्रति एक शान्त या आनन्दपूर्ण निर्भरता आदि के प्रति अपने-आप को अभ्यस्त बना लेते हैं। परन्तु गीता का आशय इन चीजों से नहीं है, यद्यपि ये अपने-अपने स्थान में उपयोगी हैं। गीता का लक्ष्य है एक ऐसी चरम-निरपेक्ष, पूर्ण एवं अटल प्रवृत्ति और मनोभाव जो आत्मा का सम्पूर्ण सन्तुलन ही बदल डालेगा। प्राणिक आवेग का मन द्वारा संयमन नहीं, अपितु अमर आत्मा की दृढ़ अविचलता ही इसका नियम है।
इसकी परीक्षा कैसे की जाए कि हम निष्काम कर्म कर भी रहे हैं या नहीं? तो इसकी कसौटी है समता। यदि हम वास्तव में निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं तो समता रहेगी ही क्योंकि कामना तो हमारे अन्दर होगी ही नहीं इसलिए कर्म प्रभावित भी कैसे होंगे। और यदि हम विचलित होते हैं तो इसका अर्थ है कि कामना अन्दर है चाहे उसे हम देख पाएँ या नहीं, परन्तु वह अन्दर विद्यमान तो है ही।
इसके लिये वह जिस कसौटी का उल्लेख करती है वह है मन और हृदय की सभी परिणामों के प्रति, सभी प्रतिक्रियाओं के प्रति, सभी घटनाओं के प्रति पूर्ण समता। यदि सौभाग्य और दुर्भाग्य, यदि मान और अपमान, यदि यश और अपयश, यदि जय और पराजय, यदि प्रिय घटना और अप्रिय घटना आकर हमें न केवल अविचलित अपितु अप्रभावित या अछूता छोड़ कर चली जाएँ, भावावेगों में मुक्त, स्नायविक प्रतिक्रियाओं में मुक्त, एवं मानसिक दृष्टिकोण में मुक्त छोड़ जाएँ, प्रकृति का कोई भी भाग जरा-सी भी उत्तेजना या कंपन के साथ प्रत्युत्तर न दे, तब समझना चाहिए कि हमारे पास वह पूर्ण मुक्ति है जिसकी ओर गीता संकेत करती है, अन्यथा नहीं। छोटी-से-छोटी प्रतिक्रिया भी इस बात का प्रमाण होती है कि हमारी साधना या हमारा अनुशासन अभी अपूर्ण है, और यह कि हमारी सत्ता का कोई भाग अज्ञान और बन्धन को अपने नियम के रूप में स्वीकार करता है और अभी तक पुरानी प्रकृति से चिपटा हुआ है। हमारी आत्म-विजय केवल आंशिक रूप से ही सिद्ध हुई है; यह हमारी प्रकृति की भूमि के कुछ भाग में या किसी हिस्से में या किसी छोटे से चप्पे में अभी तक अपूर्ण या अवास्तविक है। और अपूर्णता का वह जरा-सा कंकड़ योग के सम्पूर्ण भवन को भूमिसात् कर सकता है!
समत्वपूर्ण आत्म-भाव के ही जैसी दिखाई देने वाली कुछ अवस्थाएँ होती हैं जिन्हें गीता की गंभीर और बृहत् आध्यात्मिक समता समझ बैठने की भूल नहीं करनी चाहिये। निराशाजनित परित्याग की एक समता होती है, अभिमानजनित समता, कठोरता एवं उदासीनता की समता होती है : ये सभी अपने स्वभाव से अहंभावमय होती हैं। अवश्यंभावी रूप से ये साधनाक्रम में आती ही हैं, परंतु इन्हें अवश्य ही त्याग देना होगा अथवा सच्ची शांति में रूपान्तरित कर देना होगा। इनसे उच्चतर स्तर पर वैरागी या आत्मसंयमी की समता, धार्मिक-वृत्तिमय त्याग की या साधु-सन्तों की-सी अनासक्ति की समता तथा जगत् से विलग और उसके कर्मों के प्रति उदासीन रहनेवाली आत्मा की समता भी होती हैं। ये भी अपर्याप्त हैं; ये प्रारम्भिक प्रवेश-पथ हो सकती हैं, किन्तु आत्मा की सच्ची और पूर्ण स्वयं-सत् विस्तृत समत्वपूर्ण एकत्व में हमारे प्रवेश के लिये ये अधिक-से-अधिक प्रारम्भिक आत्म-अवस्थाएँ अथवा अपूर्ण मानसिक तैयारियाँ भर होती हैं।
अब हम इस बात तक आ गए हैं कि समता आवश्यक है, परन्तु इसे कैसे प्राप्त किया जाए? हमारी चर्चा का विषय यही था कि जब हम एकाएक ही उसे संसिद्ध नहीं कर सकते, तब फिर इस गुण को कैसे प्राप्त किया जाए? यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि जब तक अहं-भाव और कामना रहेंगे तब तक हम दिव्य कर्मी की तरह कर्म नहीं कर सकते। तो गीता ने इसके लिए सबसे पहला उपाय बताया है कामना को नियंत्रित करना जिसके लिये कि निष्काम कर्म-योग का निरूपण हुआ। और इसका मापदण्ड है समता। तो समता कैसे प्राप्त की जाए? अब उस समता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कई प्रकार की पद्धतियाँ अपनाता है कि किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, कठोरता से नियमों का पालन करना चाहिए, वैराग्य से रहना चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए, आदि। परन्तु ये सब अपूर्ण तरीके हैं जिनके परिणामस्वरूप मनोवैज्ञानिक अशांति और विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति समता प्राप्त करने के लिए इनमें से गुजरता है परन्तु ये पूर्ण नहीं हैं। गीता जिस समता की बात करती है वह तो ब्रह्म की आत्मस्थिति है, ब्रह्म की सत्ता से एक होना है। यह स्थिति तो एकदम से प्राप्त नहीं हो सकती, उस तक पहुँचने के धीरे-धीरे प्रयास ही करने होते हैं। उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अब उसके बारे में चर्चा होगी।
प्रश्न : समता के जो निम्नतर अहंपरक रूप हैं उनका हम क्या उदाहरण ले सकते हैं?
उत्तर : इसमें हम स्टोइक या तापसी जनों का उदाहरण ले सकते हैं कि चाहे कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, दुःख हो या सुख हो, ठंडा हो या गर्म हो, वे अप्रभावित रहते हैं। या फिर विरक्त व्यक्ति का यह भाव कि भगवान् ने जो कुछ भी कर दिया हो वह सदा ही सर्वश्रेष्ठ है और चाहे सारा संसार नष्ट ही क्यों न हो जाए, वह विचलित होने वाला नहीं है। परन्तु इस बाहरी दृढ़ता में भी वास्तव में तो उसके अन्दर से हलचल चल ही रही होती है। यह अहंपरक भाव ही है, कि कठोरता से व्यक्ति सभी चीजों का बाहर से निषेध करता है। इन सब भावों में या दृष्टिकोणों में अहम् का तत्त्व बहुत मजबूत रहता है।
ब्रह्म के साथ एकता से उत्पन्न होने वाली समानता एक सर्वथा भिन्त्र चीज है। उस समता में व्यक्ति कितना भी दबाव सहन कर सकता है, कितना भी भारी कर्म सहजता से कर सकता है। वहीं अहंपरक रूप से अपने ऊपर लादी गई समता में व्यक्ति एक सीमा तक तो सहन कर सकता है पर उससे अधिक आघात या थपेड़ों से वह टूट जाएगा। इसलिए इसको एक सीमा तक ही किया जा सकता है। इसी प्रकार अनेक तामसिक, राजसिक और सात्त्विक प्रकार की निवृत्ति या वैराग्य से उत्पन्न होने वाली समताएँ होती हैं जो किन्हीं आघातों के कारण, जीवन से जुगुप्सा के कारण या ऐसे ही अन्य किन्हीं कारणों से आती हैं। इसी प्रकार दार्शनिक की निवृत्ति या वैराग्यजनित समता होती है जो कहता है कि यह संसार नश्वर है अतः इसमें होने वाली घटनाओं के कारण विचलित नहीं होना चाहिए और शांत व सम बने रहना चाहिए। परन्तु ये सब प्रकार की समताएँ तो केवल मानसिक स्थितियाँ मात्र होती हैं जो कि एक सीमा से बाहर जाते ही टूट जाती हैं। ये स्थायी नहीं हो सकतीं क्योंकि इनका आधार आत्मा की वह समता नहीं होती जो कि किन्हीं भी परिस्थितियों में सुदृढ़ बनी रहती है।
यह निश्चित है कि इतने बड़े परिणाम पर तुरन्त ही और बिना किन्हीं पूर्व अवस्थाओं के नहीं पहुँचा जा सकता। पहले हमें संसार के आघातों को सहना सीखना होगा जिसमें हमारी सत्ता का केंद्रीय भाग उनसे अछूता और शान्त रहे, तब भी जब स्थूल मन, हृदय और प्राण प्रचण्ड रूप से विचलित हो रहे हों। अपने जीवन की आधारशिला पर अविचल खड़े रहकर, हमें प्रकृति की इन बाह्य क्रियाओं से आत्मा को विलग कर लेना होगा, जो कि पीछे से देखती रहती है या फिर अंदर गहराई में प्रतिरक्षित बनी रहती है। इसके बाद, निर्लिप्त आत्मा की इस शान्ति और स्थिरता को इसके उपकरणों तक फैला कर, शान्ति की किरणों को प्रकाशमय केंद्र से अधिक अन्धकारमय परिधि तक प्रसारित करना शनैः शनैः सम्भव हो जाएगा। इस प्रक्रिया में हम बहुत-सी गौण अवस्थाओं की क्षणिक सहायता ले सकते हैं; एक प्रकार की निस्पृहता या वैराग्यभाव, एक शान्त-स्थिर दर्शन, एक प्रकार का धार्मिक भावातिरेक हमें अपने लक्ष्य से किञ्चित् निकटता प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। अथवा हम अपनी मानसिक प्रकृति की कम प्रबल एवं उन्नत परन्तु तब भी उपयोगी शक्तियों को भी सहायता के लिये पुकार सकते हैं। परन्तु अन्त में हमें या तो इनका त्याग करना होगा या फिर इन्हें रूपांतरित कर इनके स्थान पर संपूर्ण समता, एक पूर्ण स्वतःसत् आंतरिक शान्ति, और यहाँ तक कि, यदि सम्भव हो तो, अपने सभी अंगों में एक पूर्ण रूप से अखंडनीय, आत्मसंस्थित और स्वतःस्फूर्त आनन्द प्राप्त करना होगा।
इसमें निहित संदेश यह है कि इस समता को हम एकाएक ही पूर्ण रूप से प्राप्त कर लें, ऐसा संभव नहीं है। अतः प्रारम्भ में - और प्रायः ही यह होता भी इसी प्रकार है - आवश्यक है कि हम अपनी सत्ता के उस गहरे भाग में, जो कि श्रीमाताजी के प्रति खुला है और उनके प्रति समर्पित है तथा जिसके संकल्प से ही हम मार्ग पर अग्रसर हुए हैं, वह अविचल बना रहे। चाहे शरीर, मन, प्राण आदि उद्विग्न होते रहें, भावनाएँ विचलित होती रहें, पर आत्मा यदि स्थिर बनी रहे तो वह हमें पथ पर लगाए रखेगी और हम चलते रहेंगे और विचलित रहते हुए भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाद में धीरे-धीरे उस गहरे भाग - जो कि श्रीमाताजी के प्रति खुला है और उनके प्रभाव के प्रति ग्रहणशील है, जिसमें उत्साह आदि हैं - की समता व उसका प्रभाव हमारी सत्ता के अन्य भागों में भी प्रवेश करने लग जाएगा। धीरे-धीरे उस गहरे भाग का प्रभाव विस्तीर्ण होकर सत्ता के अन्य भागों में फैल जाएगा जिससे कि समता आती जाएगी। और इस बीच हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों में समता पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होती परन्तु फिर भी कर्म हमारा उस ओर अग्रसर होने का एक साधन बन जाता है। क्योंकि इस स्थिति में हमारा आन्तरिक भाग तो शांत होता है इसलिये जो बाहर का विचलन है वह धीरे-धीरे कम होता जाएगा और हमारे कर्म अधिक-से-अधिक दिव्य होते जाएँगे। यही एक व्यावहारिक प्रक्रिया है क्योंकि मन, शरीर और प्राण सब एकाएक ही शान्त हो जाएँ ऐसा तो अधिकांशतः देखा-सुना नहीं जाता। 'समत्वं योग उच्यते' अर्थात् समता ही योग है। इस तरीके से ये सब बातें बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और किसी मार्ग विशेष के लिए बहुत आवश्यक हैं। समस्या यह है कि ये सारी बातें मानसिक रूप से समझने के लिए और बुद्धि में स्पष्टता लाने के लिये तो ठीक हैं परन्तु व्यावहारिक रूप से पूरा मार्गदर्शन हमें केवल श्रीअरविन्द के पत्रों से ही मिलता है। उन पत्रों में अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग निर्देश हैं, प्रत्येक व्यक्ति के स्तर के अनुसार वे सुझाव और परामर्श देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग किसी एक ही सूत्र के सहारे या फिर किसी एक सिद्धांत को लेकर समता की ओर चल पड़ें। यह पूरा विषय ही कोई इतना सरल नहीं है। यह तो एक देखने का तरीका मात्र है कि किस तरीके से भगवान् से जुड़ने पर समता आदि जैसी चीजें स्वतः ही आ जाती हैं। परन्तु इन्हें किसी भी सूत्र में बाँधा नहीं जा सकता। वास्तव में तो इतनी सब बातें केवल एक गंभीर विषय को सरल रूप से समझाने का तरीका मात्र हैं जबकि अपने-आप में विषय बहुत ही गहन और जटिल है। और सच कहें तो केवल एक ही सच्चा उपाय है कि हम श्रीमाताजी की ओर अधिकाधिक बढ़ते जाएँ और अपने समर्पण को बढ़ाते जाएँ और फिर जैसा वे चाहें वैसा होता रहे। क्योंकि कोई एक नियत-निर्धारित तरीका या सूत्र नहीं होता। ये सब बातें तो केवल बुद्धि को कुछ दिशा-निर्देश प्रदान करने में सहायक हैं, इससे अधिक नहीं।
किन्तु तब हम किसी भी प्रकार कर्म करना जारी ही कैसे रख सकेंगे? क्योंकि सामान्यतया मनुष्य इसलिये काम करता है क्योंकि उसे कोई कामना होती है अथवा वह कोई मानसिक, प्राणिक या शारीरिक अभाव या आवश्यकता अनुभव करता है; वह या तो शरीर की आवश्यकताओं से, धन-सम्पत्ति एवं मान-प्रतिष्ठा की तृष्णा से परिचालित होता है, अथवा मन या हृदय की निजी तुष्टियों की लालसा से या शक्ति (अधिकार) या सुख-भोग की उत्कट इच्छा से। अथवा वह किसी नैतिक आवश्यकता द्वारा वशीभूत होकर इधर-उधर प्रवृत्त किया जाता है, या कम-से-कम इस आवश्यकता या कामना से प्रेरित होता है कि उसके विचारों या उसके आदर्शों या उसके संकल्प या उसके दल या उसका देश या उसके देवता संसार में प्रभुत्वशाली बनें। यदि इनमें से कोई भी कामना अथवा अन्य कोई भी कामना हमारे कार्य की परिचालिका नहीं होती तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त प्रोत्साहन या प्रेरकशक्ति ही हटा ली गयी है और तब स्वयं कर्म भी अनिवार्य रूप से बन्द हो जाएगा। गीता इसका उत्तर दिव्य जीवन के अपने तीसरे महान् रहस्य को खोलकर देती है। अवश्य ही समस्त कर्म एक अधिकाधिक ईश्वरोन्मुख और अन्ततः ईश्वर-अधिकृत चेतना में रहते हुए करने होंगे, हमारे कर्म भगवान् के प्रति यज्ञ-रूप होने चाहिये, और अन्ततः हमारी सम्पूर्ण सत्ता का, मन, संकल्प-शक्ति, हृदय, इंद्रिय, प्राण और शरीर, सब का - एकमेव के प्रति समर्पण अवश्य ही ईश्वर-प्रेम और ईश्वर-सेवा को ही हमारे कर्मों का एकमात्र प्रेरक-भाव या हेतु बना देगा। प्रेरक-शक्ति का और कर्मों के स्वरूपमात्र का यह रूपान्तर ही निस्संदेह गीता का प्रधान विचार है; कर्म, प्रेम और ज्ञान के इसके अद्वितीय समन्वय का यही आधार है। अन्त में, कामना नहीं, अपितु सनातन की सचेतन रूप से अनुभूत इच्छा ही हमारे कर्म की एकमात्र परिचालिका और इसके सूत्रपात की एकमात्र प्रवर्तक रह जाती है।
समता, हमारे कर्मों के फल की समस्त कामना का त्याग, हमारी प्रकृति और समष्टि-प्रकृति के परम् प्रभु के प्रति यज्ञ-रूप से कर्म करना, - ये ही गीता की कर्मयोग-प्रणाली में ईश्वरोन्मुख प्रवेश-प्राप्ति के तीन प्रथम साधन हैं।
III. यज्ञ का महत्त्व
यज्ञ का विधान वह सार्वजनीन दिव्य क्रिया है जिसे इस जगत् के आदि में ब्रह्माण्ड के पूर्ण एकत्व (लोकसंग्रह) के प्रतीक के रूप में प्रकट किया गया था। इसी विधान के आकर्षण से एक दिव्यीकारक, एक रक्षक शक्ति इस अहंकारमय और स्वतः-विभक्त सृष्टि की भूलों को मर्यादित करने और उन्हें संशोधित तथा उत्तरोत्तर दूर करने के लिये अवतरित होती है। यह अवतरण, पुरुष का यह यज्ञ, अर्थात् 'दिव्य आत्मा' का अपने-आप को शक्ति और जड़-प्रकृति के अधीन कर देना जिससे कि इन्हें अनुप्राणित और प्रकाशयुक्त कर सके - निश्चेतना और अविद्या के इस संसार से उद्धार का बीज अथवा मूल रहस्य है।
यज्ञ का रहस्य इसमें असंदिग्ध रूप से बिल्कुल स्पष्ट ही दे दिया गया है। भगवान् ने तीसरे अध्याय में कहा है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तब उन्होंने कहा कि यज्ञ के द्वारा तुम अपने-आप को परिपुष्ट करो। यज्ञ का अर्थ है एकता का सिद्धांत।
श्रीअरविन्द का कहना है कि संसार में जो इतना वैविध्य है, जो विभिन्नता है उसका आधार है एकता। एकता जितनी ही अधिक महान् होगी उतनी ही अधिक विभिन्नता, विविधता वहन की जा सकती है, फिर उसमें कोई खतरा नहीं है, वैसे ही जैसे कि यदि हमारा कोई अत्यंत प्रिय है वह हमारे किसी भी व्यवहार से खिन्न नहीं होता, भले उसे हम अनदेखा कर दें, उसकी उपेक्षा कर दें, क्योंकि हमारे प्रेम का आधार इतना सुदृढ़ होता है इसलिए हमारे किसी भी व्यवहार से उसे वास्तव में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। हाँ, यदि प्रेम का आधार दृढ़ न हो तब फिर सभी बातों का बड़ा ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, भगवान् की एकता इतनी महान् है कि यह सारी गोचर और अगोचर विविधता भी उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इन सबके अंदर एकता की रक्षक शक्ति निहित है। यह यज्ञ का मूल रूप है, उसका मूल तत्त्व है।
इस एकता के कारण ही स्रष्टा और स्रष्ट जगत् तथा इसमें व्याप्त सभी चराचर जीव और पदार्थ सहज रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। यहाँ इस ब्रह्माण्ड में परमात्मा चूँकि एकत्व हैं और उन्होंने ही इस विविधता का रूप ले लिया है, और स्वयं वे अनंत परमात्मा इसमें व्याप्त हैं, इसलिए वे इससे विलग कैसे हो सकते हैं। और इसी कारण वे स्वयं हो अपने इस विविधतापूर्ण रूप में अंतर्निहित हैं। अब परमात्मा यह जड़तत्त्व कैसे बने? उन्होंने स्वयं अपने-आप को ही इस रूप में परिवर्तित कर दिया। इसलिए जब स्वयं परमात्मा उसमें व्याप्त हैं इसलिए जड़ जगत् भी उनकी ओर आकर्षित होने को बाध्य है।
---------------------------------------------------------
* यह आत्मदान है। यह वह शब्द है जिसे गीता आत्मदान के लिए प्रयुक्त करती है। भेद केवल यह है, यज्ञ परस्पर होने वाली चीज है... भगवान् ने स्वयं को 'जड़-तत्त्व' के अंदर उत्सर्ग कर दिया है जिससे कि जड़तत्त्व में, जो निश्चेतन बन गया था, चेतना जागृत करें। और यही है वह यज्ञ, जड़तत्त्व में भगवान् का उत्सर्ग, अर्थात् जड़तत्त्व में उनका प्रकीर्णन या बिखराव जो कि भगवान् के प्रति जड़तत्त्व के यज्ञ का औचित्य सिद्ध करता है और इस यज्ञ को आवश्यक बना देता है; क्योंकि यह तो एक ही जैसी पारस्परिक और प्रतिक्रियात्मक क्रिया है। क्योंकि जड़तत्त्व को दिव्य चेतना के प्रति जागृत करने के लिए भगवान् ने स्वयं को जड़तत्त्व में उत्सर्ग कर दिया है और जड़तत्त्व में सर्वत्र अपने आप को इस प्रकार प्रकीर्ण कर दिया है कि जड़तत्त्व स्वयमेव ही बाध्य है कि वह स्वयं को भगवान् के प्रति उत्सर्ग करे। यह एक पारस्परिक और अन्योन्य यज्ञ है।
और यही गीता का महान् रहस्य है: 'जड़-तत्त्व' के मर्म तक में भागवत् 'उपस्थिति' की अभिपुष्टि। और, इसी कारण, 'जड़-तत्त्व' को अवश्य स्वतः ही भगवान् के प्रति उत्सर्ग करना होगा, स्वतः, यहाँ तक कि अचेतन रूप से भी भले कोई ऐसा चाहे या नहीं, यही होता है।
केवल, जब यह अचेतन रूप से किया जाता है तब मनुष्य को यज्ञ का हर्ष नहीं प्राप्त होता; जबकि यदि यह सचेतन रूप से किया जाता है तो मनुष्य को यज्ञ का हर्ष प्राप्त होता है जो कि परमोच्च हर्ष है।
इसलिए जो निवर्तन (involution) हुआ उसी के प्रत्युत्तर में क्रमविकास (evolution) हुआ। यह चेतना जड़तत्त्व में अंतर्निहित है। इसलिए जड़तत्त्व स्वयं चाहे या न चाहे, पर अपने अंदर से वह अपने मूल स्वरूप परमात्मा की ओर पुनः जाने के लिए बाध्य होता है। जड़तत्त्व की यह सारी प्रक्रिया चलती रहती है। पर मनुष्य में जब यह प्रक्रिया सचेतन हो जाती है, तब वह इस यज्ञ के आरोहण का आनंद ले सकता है। जब तक उसे इस आरोहण का भान नहीं होता और अवश रूप से वह इसे करता रहता है, तब तक उसे इसका पूरा आनंद नहीं मिलता।
आरंभ में मनुष्य इसलिए कर्म करता है कि उसे किसी आवश्यकता या कामना की पूर्ति करनी होती है। यदि भोजन चाहिये तो अमुक क्रिया करनी होगी, कुछ और चीज की आवश्यकता हो तो उसके अनुसार क्रिया करनी होगी। ये सब तो मनुष्य को अवश रूप से करने होते हैं। इसलिए व्यक्ति को जो कुछ प्राप्त करना होता है उसके लिए उसे उतनी ऊर्जा व्यय करनी होती है, क्योंकि यज्ञ का तत्त्व तो निहित है इसलिए आदान-प्रदान तो रहेगा ही। इस आदान-प्रदान के द्वारा ही मनुष्य विकसित हो सकता है और अपने सच्चे स्वरूप में बढ़ सकता है। ऐसा न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी प्रगति नहीं की जा सकती। इस आदान-प्रदान को रोका जा ही नहीं सकता। पर जब व्यक्ति इसका मूल सिद्धांत समझ जाता है, तब वह प्रसन्न होकर इसे करता है। और जब प्रसन्न होकर व्यक्ति यह आदान-प्रदान करता है तब यज्ञ शुरू हो जाता है। इससे अधिक आनंद और किसी चीज में नहीं है। अपने-आप को दे देने में जो आनंद है वह अद्भुत है। हमारे सारे दुःख-कष्ट, पीड़ा-यंत्रणा केवल अहं के कारण आते हैं, इसलिये आते हैं क्योंकि व्यक्ति को स्वयं से लगाव होता है। हमने अपने मनोवैज्ञानिक जीवन में इतनी बेड़ियाँ डाल रखी होती हैं कि उनके कारण आरोहण मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति कहता है 'मेरा तो अपने पुत्र से बड़ा मोह है' या फिर 'मुझसे उस व्यक्ति का दुःख नहीं देखा जाता। पर पुत्र तो उसके अपने अहं का रूप ही तो है। और दूसरे व्यक्ति के दुःख का भाव भी अहं के कारण ही है। इस सबका मूल कारण है कि व्यक्ति अपने अहं से मुक्त नहीं है। क्योंकि यदि व्यक्ति किसी गहरी चीज के प्रति समर्पित हो तो फिर वह इन बाह्य चीजों या घटनाओं से इस तरह प्रभावित नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमने इतनी बेड़ियाँ डाल रखी होती हैं जिनके कारण हमारे यज्ञ का आरोहण नहीं हो पाता।
यह यज्ञ भी तामसिक, राजसिक व सात्त्विक, तीन प्रकार का बताया गया है। तामसिक यज्ञ तब है जब व्यक्ति अधिक-से-अधिक फल चाहता है परंतु ऊर्जा कम-से-कम देना चाहता है, और केवल बाध्य होकर ही अपनी ऊर्जा व्यय करता है। राजसिक यज्ञ में व्यक्ति इसलिए कर्म करता है कि यदि वह किसी के लिए काम करेगा तो बदले में उसे भी लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में, सात्त्विक प्रकार के यज्ञ में व्यक्ति इसकी परवाह नहीं करता कि सामने वाला उसे लाभ पहुँचाएगा या नहीं, उसे तो जो उचित कर्म है वह करना होता है, न कि फल की आशा से। अब, निलैगुण्य यज्ञ वह है जिसमें व्यक्ति को कर्म करने या न करने पर कोई आग्रह नहीं होता, जिस प्रकार जगदम्बा चाहती हैं वैसे ही वह कर्म करता है, उसी प्रकार के विचार आने लगते हैं, वे ही कर्म होने लगते हैं, स्वतः वे ही भावनाएँ आने लगती हैं। व्यक्ति सहज रूप से परमात्मा के प्रति खुला होता है और जैसा वे चाहते हैं वैसी ही क्रिया करता है। क्योंकि भगवान् की परा प्रकृति ही है जो सभी कुछ करती है। 'अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च' अर्थात् 'मैं स्वयं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और ईश्वर हूँ।' 'भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वर' 'अर्थात् सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता मैं स्वयं हूँ और सभी लोकों का महान् ईश्वर हूँ।' 'सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शान्तिमरिच्छति' और 'मैं ही सभी भूतों का सुहृद हूँ यह जानकर व्यक्ति शान्ति प्राप्त कर लेता है।' क्योंकि जब मैं स्वयं ही महान् ईश्वर हूँ और तुम्हारा सुहृद हूँ तो फिर तुम्हारे साथ कोई गलत काम हो ही कैसे सकता है।
इस प्रकार यज्ञ का विधान तो सृष्टि में अंतर्निहित है। यदि कोई अपने को आत्म-निर्भर या अपने-आप में एक स्वतंत्र इकाई मानना चाहे तो यह चल नहीं सकता, क्योंकि सभी कुछ तो एक है। यदि शरीर के अंदर सभी अंग अपने को स्वतंत्र मान लें तो यह बात चल नहीं सकती। वैसे ही ब्रह्माण्ड में सभी चीजें परस्पर जुड़ी हुई हैं। यदि ऐसा न हो तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ आदान-प्रदान के बिना कुछ भी अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। शरीर में भी आदान-प्रदान चलता रहता है, जैसे कि साँस लेने से प्राण-वायु आती है, रक्त उसका सभी अंगों तक संचार करता है, सभी अंग अपना-अपना काम करते हैं और एक-दूसरे की क्रिया को परिपूरित करते रहते हैं। इस आदान-प्रदान से ही शरीर की अभिवृद्धि और विकास होता है और शरीर सुचारू रूप से चलता है।
श्रीअरविन्द कहते हैं कि गीता जिस यज्ञ की बात करती है वह उस समय विशेष से संबंधित या कोई बाह्य अनुष्ठान ही नहीं है। यह तो एक ऐसा सिद्धांत है जो सभी कुछ के अंदर निहित है, इस ब्रह्माण्ड का मूलभूत विधान है। यह कोई परिपाटी ही नहीं है। इसलिए गीता के यज्ञ विधान का अर्थ बहुत ही गहन है। इस चौथे अध्याय में तो इस बात में कोई संदेह ही नहीं बचता कि गीता केवल किसी प्रकार के बाह्य यज्ञ की ही बात नहीं कर रही है।
गीता का संपूर्ण कर्म-सिद्धांत उसके यज्ञसंबंधी विचार पर आश्रित है और यह वस्तुतः ईश्वर, जगत् और कर्म के बीच सनातन संयोजक सत्य को अपने में समाहित रखता है। सामान्यतया मानव-मन अस्तित्व के बहुमुखी सनातन सत्य की केवल अपूर्ण या आंशिक धारणाओं और दृष्टिकोणों को पकड़ता है और उन्हीं के आधार पर जीवन, आचारनीति और धर्मसम्बन्धी विभिन्न सिद्धांतों को गढ़ डालता है, तथा उनके इस या उस लक्षण या रूप पर बल देने लगता है। परंतु मन जब कभी महान् प्रकाश के युग में अपने जगत्-ज्ञान के साथ भागवत् ज्ञान और आत्मज्ञान के पूर्ण और समन्वयात्मक सम्बन्ध की ओर लौटता है तो उसका हमेशा ही इन अपूर्ण सिद्धांतों की किसी पूर्णता की ओर पुनर्जागृत होना तय है। गीता की शिक्षा वेदान्त के इस मूल सत्य पर आश्रित है कि सारी सत्ता एक ही ब्रह्मसत्ता है और सारी अस्तित्वमान सत्ता ब्रह्म का चक्र है; एक ऐसी दिव्य गति है जो भगवान् से आरंभ होती है और भगवान् की ओर लौट जाती है। सभी कुछ प्रकृति की व्यंजक क्रिया है और प्रकृति भगवान् की वह शक्ति है जो अपने कर्मों के स्वामी और अपने रूपों के अंतर्यामी दिव्य पुरुष की चेतना और इच्छा (संकल्प) को ही कार्यान्वित करती है। उस (अंतर्यामी दिव्य पुरुष) की प्रसन्नता के लिये ही वह रूपाकृतियों में और प्राण तथा मन के कर्मों में लीन होकर अवतीर्ण होती है और मन-बुद्धि और आत्म-ज्ञान के द्वारा उस अंतर्यामी आत्मा (दिव्य पुरुष) के सचेतन अधिकार की स्थिति तक पुनः लौट जाती है। पहले आत्मतत्त्व का, जो कुछ भी वह है तथा नामरूपात्मक विकास से उसका जो कुछ भी अभिप्राय है उस सब का, प्रकृति में अंतर्वलयन (involution) होता है; इसके बाद आत्मतत्त्व का विकास होता है, अर्थात् वह जो कुछ है, उसका जो अभिप्राय है, और जो अदृष्ट होने पर भी नामरूपात्मक सृष्टि द्वारा संकेत रूप से व्यक्त किया जाता है, वह सब प्रकट होता है। प्रकृति का यह चक्र जैसा अभी है वैसा कभी न हो पाता यदि पुरुष तीन शाश्वत अवस्थाओं को एक साथ धारण कर के बनाये न रखता, क्योंकि प्रत्येक अवस्था इस कर्म की समग्रता के लिये आवश्यक है। पुरुष के लिए अपने-आप को क्षररूप में प्रकट करना अपरिहार्य है, और वहाँ हम उसे सीमित, अनेक, सर्वभूतानि के रूप में देखते हैं। यह पुरुष हमें अपनी अनन्त विभिन्नताओं और नानाविध संबंधों से युक्त असंख्य प्राणियों के सीमित व्यक्तित्वों के रूप में दिखाई देता है, और फिर यही पुरुष हमें इन सब प्राणियों के पीछे होनेवाली देवताओं की क्रियाओं के मूलतत्त्व और उनकी शक्ति के रूप में दिखायी देता है, - अर्थात् भगवान् की उन वैश्वशक्तियों और गुणों के रूप में जिनके द्वारा जगत् के जीवन का संचालन होता है और जो हमारी दृष्टि के लिए एकमेव सत्ता के भिन्न-भिन्त्र वैश्व रूपों का गठन करते हैं, अथवा हो सकता है कि ये सब (देवता) एक ही परम् पुरुष के व्यक्तित्व के विविध आत्म-निरूपण हों। फिर, सभी रूपों और सत्ताओं के पीछे और इनके अन्दर हमें यह भी प्रतीति होती है कि एक गूढ़, अक्षर, अनन्त, देश-कालातीत, नैयक्तिक, अव्यय सत् विद्यमान है, जो सारे अस्तित्व का एक अखंड आत्मतत्त्व है, जिसमें ये सब बहुत्व अपने-आप को यथार्थतः एक पाते हैं। अतएव उस एक पुरुष-भाव में लौट आने पर व्यष्टिगत पुरुष का सक्रिय सीमित व्यक्तित्व यह पाता है कि इस अखंड अनंत से जो कुछ निःसृत होता है और उसके द्वारा जो कुछ धारण किया जाता है वह उसकी अक्षर और अलिप्त ऐक्य की शांति और समस्थिति में तथा विश्वव्यापकता की प्रशांत विशालता में अपने-आप को मुक्त कर सकता है। या फिर वह व्यष्टिगत सत्ता से इसमें पलायन भी कर सकता है। परन्तु सबसे परम् गुह्य 'उत्तमं रहस्यं' है पुरुषोत्तम। यह परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो अनन्त और सीमित दोनों अवस्थाओं को धारण रखते हैं और जिनमें व्यक्ति और निर्व्यक्ति (सगुण और निर्गुण), एकमेव आत्मतत्त्व (ब्रह्म) और अनेक भूत, सत्ता और उसकी बाह्य अभिव्यक्ति, संसार-कर्म और विश्वातीत शान्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये सब-के-सब मिलकर एकत्व को प्राप्त होते हैं, एक साथ और अलग-अलग भी धारण किये जाते हैं। परमेश्वर के अन्दर सब पदार्थ अपना गुह्य सत्य और परम् समन्वय प्राप्त करते हैं।
इसमें बातें तो बहुत हैं परन्तु मोटे रूप में जितना हम समझ सकते हैं, उसे समझने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि ये विचार सहज ही पकड़ में नहीं आते। यहाँ बता रहे हैं, और यही हमारे सारे वेद, वेदांत भी कहते हैं कि सारे ब्रह्माण्ड में केवल एक ही सत्ता है - 'एकमेवाद्वितीयम्'। और वह 'सत्ता' अपनी अंतर्तम गहराइयों में व्यक्ति स्वयं ही है। जब व्यक्ति अपनी अंतर्तम गहराइयों में जाता है तब वह पाता है कि सभी शरीरों में और सभी कुछ में वह स्वयं ही व्याप्त है, उसके अतिरिक्त दूसरा न तो कोई है और न कभी था और चूंकि उसके अतिरिक्त किसी दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है इसलिए वह स्वतः ही सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह परम् सत्य है कि केवल 'एकमेवाद्वितीयम्' का ही अस्तित्व है तो फिर यह सब दृश्य-प्रपंच क्या है। इसे सोचने और समझने के अनेक तरीके हैं। एक तरीका जो गीता बता रही है वह यह है कि मान लें कि आप अकेले ही हैं, आपके अतिरिक्त अन्य किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है और आपके पास भंडार भरे हुए हैं। अब, आपके अंदर जिज्ञासा उठती है कि इस सब को देखा जाए, इसका निरीक्षण किया जाए। आप इसे देखते और संभालते हैं। इस सब चर्चा में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि यह सब केवल समझने के लिये ही है क्योंकि हम मनुष्य अपनी मानसिक चेतना से इससे अधिक कल्पना नहीं कर पाते। तो, हमारी परंपरा में सदा ही यह मानते हैं कि एक तो परमात्मा स्वयं हैं और दूसरी है उनकी चित्-शक्ति, या फिर उनकी संकल्प-शक्ति, क्रिया शक्ति। इस प्रकार परमात्मा ने स्वयं को दो भागों में बाँट लिया क्योंकि बिना इसके तो कोई सृष्टि हो नहीं सकती। सृष्टि के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, एक है विषय अर्थात् वह पदार्थ जिसे देखा जाए और एक है उसे देखने वाला द्रष्टा या फिर आत्मपरक चेतना। यदि पदार्थ है पर उसे देखने वाला कोई नहीं है तो उसके होने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। और यदि द्रष्टा है पर पदार्थ नहीं है तो सृष्टि होती ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने अपने-आप को खेल करने के लिए दो भागों में विभक्त कर लिया। एक भाग तो वह है जिसमें उनकी सारी समृद्धताएँ, सारी भव्यताएँ आदि सभी कुछ समाहित हैं। और दूसरे भाग में उन्होंने द्रष्टा भाव अपना लिया ताकि इस सारी भव्यता और समृद्धता का अवलोकन कर सकें। और वास्तविक सृष्टि का अर्थ यही है कि जहाँ भी वे अपनी दृष्टि डालते हैं वहीं पर वे भव्यताएँ प्रकट हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। जैसे कि चीजें तो बहुत हैं परन्तु जिस समय आप जिस चीज को देख रहे होते हैं उस समय आपके लिए वही चीज अस्तित्व रखती है। जिस प्रकार हम जिस सड़क से जा रहे हैं उस समय हमें वही प्रत्यक्ष होती है, बोध भी उसी का होता है, उसी को महसूस करते हैं, अन्यथा सड़कें तो और भी बहुत-सी हैं। यही बात सृष्टि के लिये भी है। जो सृष्टि हमें दिखाई देती है उसमें प्रकृति का काम है कि वास्तव में जो प्रभु की भव्यताएँ हैं, उनका सत्स्वरूप है, उनका जो आंतरिक स्वरूप है उसे प्रकट करे। अब मान लें कि आप अकेले ही हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और आपने अपनी इच्छा-शक्ति को निर्देश दिया कि आपके रूप को प्रकट कर के दिखाए कि आप क्या हैं, कैसे हैं क्योंकि आपको अपने-आप को देखने में आनंद आता है। अतः आपकी इच्छा-शक्ति इस कार्य को करने में अपनी सारी सामर्थ्य लगा देती है। और वह इस-इस तरीके के रूप बनाती है, ऐसी विराट् सृष्टि करती है जिसमें किसी-न-किसी रूप में, किसी-न-किसी चीज में, कहीं न कहीं आपकी कोई बात, कोई चीज पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि उसे तो अंतरंग रूप से आपके स्वरूप का पता है क्योंकि वह तो आपकी ही क्रियाशक्ति है, इच्छाशक्ति है, संकल्पशक्ति है, आपकी ही चेतना है। अब हमें जो सृष्टि यहाँ गोचर हो रही है उसमें हमें यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ने स्वयं को अनंत रूपों में प्रकट किया है। और न जाने कहाँ-कहाँ, कितने-कितने ब्रह्माण्ड हैं और उनमें क्या-क्या हो रहा है, उनके बारे में हमें पता भी नहीं है। यह इतनी विशाल चीज है जिसको हम अनंत नजरियों से देखें, अनंत तरीकों से देखें तो भी उनके स्वरूप का, उनके तत्त्व का, उनकी अंतर्वस्तु का कोई अंत नहीं है। अब प्रकृति ने परमात्मा के विभिन्न रूप बनाए जिससे वे उन रूपों में स्वयं को देख सकें। गीता में भी उल्लेख है 'सर्वभूतानि' - जिसमें असंख्यों तरीके की चीजें हैं - जिसमें जड़तत्त्व भी है, पशु-पक्षी भी हैं, मनुष्य आदि भी हैं। संसार को देखने का इन सबका अपना-अपना नजरिया है। पक्षी अपने तरीके से देखते हैं, पशु अपने तरीके से देखते हैं, प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने तरीके से देखता है। और ये सभी चाहे किसी भी नजरिये से क्यों न देख रहे हों, परंतु उस परम तत्त्व के किसी-न-किसी अंश को अवश्य देख रहे होते हैं। हाँ, यह कह सकते हैं कि कोई अधिक समझदारी से देखता है, तो कोई कम समझदारी से देखता है परन्तु सब देखते उसी की छवि को हैं। कोई उसे धुँधले तरीके से देखता है, किसी की उसको देखने की छवि काली है, किसी की सफेद है और किसी की रंगीन है। ये सारे रूप जो प्रकृति ने सृष्ट किये वे उन्हीं परमात्मा को प्रकट कर रहे हैं, उनको पहचान करा रहे हैं। इस पहचान करने की प्रक्रिया में चाहे कोई कहीं से भी शुरू करे पर वह नजरिया अंतिम नहीं होता। चीजों की सृष्टि कैसे होती है इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मनुष्य अनेक विचारों के अनुसार - जैसे कि राष्ट्रीयता का विचार, जाति का विचार आदि; अनेक व्यवस्थाओं के अनुसार - जैसे कि आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था आदिः अनेक सिद्धांतों के अनुसार जोता है। परंतु ये चीजें किसी बंदर की चेतना के लिए अस्तित्व ही नहीं रखतीं। और फिर किसी पत्थर से तो इसे समझने की अपेक्षा करना बिल्कुल ही निरर्थक बात है। इसलिए ज्यों-ज्यों चेतना का विकास होता है त्यों-ही-त्यों परमात्मा के स्वरूप का, उनके तत्त्व का, उनकी समृद्धताओं का अधिकाधिक पता लगता जाता है।
इस प्रकार, आरंभ में हमें जैसी प्रतीति होती है, उसे गीता क्षर-पुरुष की संज्ञा देती है। उसके बाद ज्यों-ज्यों व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास होता है त्यों-ही-त्यों उसमें विशालता आती जाती है और वह चीजों को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखने लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा आरंभ में अपनी सीमित बुद्धि से ही विश्व को देखता है, और उसकी दुनिया भी बहुत छोटी-सी होती है, परंतु ज्यों-ज्यों वह वर्धित होता है, ज्यों-ज्यों उसका मानसिक विकास होता है और ज्यों-ज्यों वह अधिक परिष्कृत और सुसंस्कृत होता है त्यों-ही-त्यों विश्व उसके लिए बदलता जाता है। वह उसे भिन्न रूप से और अधिक समृद्ध रूप से देखने लगता है। एक सीमित दृष्टिकोण का व्यक्ति सीमित रूप से ही चीजों को देखता है। फिर ज्यों-ज्यों व्यक्ति सचेतन होता जाता है, या फिर ध्यान आदि क्रियाओं के द्वारा जब वह अपनी सूक्ष्म और प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करता है, उन्हें वर्धित करता है त्यों-ही-त्यों उसे एक और अधिक विशाल जगत् दिखाई देता है जो कि बिना इन शक्तियों को जागृत किये दिखाई देना संभव नहीं था। इन इन्द्रियों की शक्तियों को ही देवता कहा जाता है। जैसे किसी वैज्ञानिक को अनेक प्रकार के तत्त्वों का ज्ञान होता है परन्तु किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो उन तत्त्वों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अब किसी वैज्ञानिक के लिए वे तत्त्व इसलिए प्रकाश में आए क्योंकि उसने अपनी चेतना को उनकी खोज में लगाया और उन्हें प्रकट किया अन्यथा वे तत्त्व कभी भी प्रकाश में नहीं आते। इसीलिए इस जगत् को 'लोक' कहते हैं अर्थात् जिस चेतना के स्तर से हम इसका अवलोकन करते हैं वह हमें वैसा ही गोचर हो जाता है और उसी के अनुसार चीजें हमारे सामने प्रकट कर देता है। और ये सारी चीजें देवताओं (अर्थात् हमारी मनोवैज्ञानिक शक्तियों) के साथ आदान-प्रदान करने से विकसित होती हैं। हमारे वेदों में यह वर्णन है कि पहले व्यक्ति चीजों को एक सीमित दृष्टिकोण से देखता है परन्तु ज्यों-ज्यों उसकी मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ विकसित होती हैं वह चीजों को और अधिक विशाल दृष्टिकोण से देखने लगता है। चूंकि मनुष्य की सामान्य चेतना कोई अंतिम नहीं है, वह चेतना के अनंत स्तरों की शीर्ष अवस्था नहीं है, सदा ही उसमें व्यक्ति उत्तरोत्तर आरोहण कर सकता है। इसलिए चेतना ज्यों-ज्यों विकसित होती जाती है त्यों-त्यों वह और अधिक विशाल और समृद्ध जगत् देखता है, और उसे वे शक्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगती हैं जो किसी साधारण चेतना में दिखाई नहीं देतीं। और इस प्रकार यह आरोहण चलता जाता है।
इसका दूसरा पहलू यह है कि जब व्यक्ति की आत्म-उन्नति होती है, तो उसके इंद्रिय-बोध, मन, बुद्धि आदि भागों के बोध अधिकाधिक विशाल होते जाते हैं और अन्त में जब वह विशाल होकर इन सबसे ऊपर उठ जाता है तो आखिर में उसे सारा ब्रह्माण्ड नजर आने लगता है, और फिर सारा ब्रह्माण्ड उसे स्वयं के भीतर ही दिखाई देने लगता है। व्यक्ति को इस प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। उसे वैश्विक सत्ता का अनुभव होने लगता है। उससे भी परे व्यक्ति किसी ऐसी सत्ता के या किसी ऐसी चीज के संपर्क में आ जाता है जिसका कि यह वैश्विक सत्ता भी एक रूप मात्र ही है, एक अंग है। तब व्यक्ति जान जाता है कि इस विश्व में जो कुछ भी गोचर हो रहा है वह उसी सत्ता का रूप है, जो शाश्वत है, अनंत है, आनंदमय है। यह एक तीसरा तत्त्व शामिल हो जाता है। इन तीनों से संसार बना है। इनमें एक चौथा तत्त्व है जो सबसे महत्त्वपूर्ण है। वह यह है कि चेतना के इस विस्तार में यदि व्यक्ति और भी आगे जाए तो एक समय आएगा जब वह देखेगा कि परम प्रभु वह स्वयं ही है, और वही इन सब चीजों में विभक्त हुआ है और यह सारा खेल उसी का है। और उसे अनुभव होगा कि उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। यह स्वयं पुरुषोत्तम का भाव है। और सब कुछ उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं के निमित्त हो रहा है। उस चेतना से मनुष्य जुड़ सकता है। गीता का कहना है कि 'क्षर और अक्षर से ऊपर उठ कर पुरुषोत्तम अर्थात् मेरे पास आ (मद्भावम् आगताः), अर्थात् मेरा जो भाव है उसी भाव में तू भी आ। और जब तू मेरी चेतना से जुड़ जाएगा तो तुझे मेरा भाव प्राप्त हो जाएगा।'
और हमारी प्राचीन परंपरा में चतुर्वर्णों का विभाजन साधना के दृष्टिकोण से किया गया था, किसी व्यापारिक या पेशे के दृष्टिकोण से नहीं। कालांतर में जब इस व्यवस्था का ज्ञान लुप्त हो गया तब इसे जन्म के आधार पर ही मान लिया गया और वंशपरंपरा के आधार पर पेशे का निर्धारण होने लगा। परन्तु यह चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं कि ये चारों वर्ण तो जगदम्बा की चार महान् शक्तियों की क्रिया पर आधारित हैं। यद्यपि श्रीमाताजी की अनंत शक्तियाँ हैं परंतु अभिव्यक्ति में चार ही प्रधान रूप से क्रियाशील हैं। और प्रत्येक व्यक्ति में यों तो चारों ही शक्तियाँ विद्यमान होती हैं परंतु आरंभ में अधिकांश में कोई एक या दो ही अधिक प्रभावी होती हैं। परंतु यज्ञ के आरोहण के द्वारा व्यक्ति अंततः इन चारों शक्तियों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। गीता कहती है कि प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि वह स्वामी की स्थिति तक, अर्थात् पुरुषोत्तम भाव तक पहुँच सके। और इस स्थिति तक पहुँचने का मार्ग है यज्ञ जिसकी विस्तृत चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं। तो इस प्रकार हम क्षर, देवता, अक्षर, पुरुषोत्तम-संबंधी इस विषय को समझ सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की सारी व्यवस्था इसी दृष्टिकोण से बनाई गई थी कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप तक यथाशीघ्र ले जाया जा सके।
अवश्य ही कर्मों का सारा सत्य सत्ता के सत्य पर ही निर्भर होता है। अवश्य ही संपूर्ण सक्रिय जीवन अपनी अंतरतम यथार्थता में प्रकृति द्वारा पुरुष को निवेदित एक कर्म-यज्ञ है। यह प्रकृति का अपने अन्दर रहने वाले सीमित बहुपुरुष की कामना को उस एक परम् और अनन्त पुरुष को भेंट चढ़ाना है। जीवन एक यज्ञवेदी है जिस पर प्रकृति अपने कर्मों और कर्मफलों को लाती और उन्हें भगवान् के उस रूप के सामने रखती है जिस रूप तक उसकी चेतना पहुँच पायी हो और इस यज्ञ से उस सब फल की कामना की जाती है जिसे शरीर-मन-प्राण में रहनेवाला जीव अपना तात्कालिक या परम श्रेय मानता हो। प्रकृतिस्थ पुरुष अपनी चेतना और आत्मसत्ता के जिस स्तर तक पहुँचा हुआ होता है उसके अनुरूप ही उस ईश्वर का स्वरूप होगा जिसे वह पूजता है, वैसा ही आनन्द होगा जिसे वह ढूँढ़ता है और वैसी ही आशा होगी जिसके लिये वह यज्ञ करता है। प्रकृतिगत क्षर पुरुष की प्रवृत्ति में सारा व्यवहार पारस्परिक आदान-प्रदान है और अवश्य ही होगा क्योंकि सत्ता एक है और इसके विभाजनों को अपने-आप को परस्पर निर्भरता के किसी ऐसे विधान पर स्थापित होना होता है जिसमें प्रत्येक दूसरे के सहारे बढ़ता है और सभी के सहारे जीता है। जहाँ यज्ञाहुति स्वेच्छापूर्वक नहीं दी जाती वहाँ प्रकृति बलात् ऐसा करा लेती है, वह अपने जीवन-विधान की पूर्ति कर लेती है। पारस्परिक आदान-प्रदान जीवन का नियम है जिसके बिना वह एक क्षण के लिये भी बना नहीं रह सकता और यह तथ्य संसार पर उस भगवान् के सर्जनशील संकल्प की छाप है जिसने संसार को अपनी सत्ता में अभिव्यक्त किया है, और यह इस बात का प्रमाण है कि यज्ञ को उनका शाश्वत साथी बनाकर प्रजापति ने इन सब प्रजाओं की सृष्टि की थी। यज्ञ का यह विश्वव्यापक विधान इस बात का चिह्न है कि यह संसार ईश्वर तत्त्व का है और ईश्वर का ही इस पर अधिकार है, जीवन उसी का राज्य और अर्चना-मंदिर है, किसी स्वतंत्र अहंकार की आत्म-संतुष्टि का क्षेत्र नहीं है; अहंकार की संतृप्ति नहीं, - क्योंकि वह तो जीवन का असंस्कृत और अंधकारमय आरम्भमात्र है, अपितु भगवान् की खोज, निरंतर विस्तृत होते यज्ञ के द्वारा भगवान् और अनन्त की पूजा और उनका अन्वेषण, और उस यज्ञ की परिणति पूर्ण आत्मज्ञान पर प्रतिष्ठित पूर्ण आत्मदान में होती है, और अंततः जीवन का अनुभव इसी आत्मदान तक ले जाने हेतु अभिप्रेत होता है।
यज्ञ का विचार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि पुरातन समय में तो भारतीय संस्कृति ने आरम्भ किया हो पर अब उसका समय नहीं रहा हो। गोता में निहित यज्ञ का सिद्धांत तो एक ऐसी मूलभूत बात है जिसके बिना सारा ब्रह्माण्ड क्षण भर भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। क्योंकि यज्ञ का सिद्धांत तो इसमें आरंभ से ही निहित है और उसी के आधार पर यह सृष्टि हुई है। इसमें आधारभूत तथ्य यह है कि परमात्मा केवल एक हैं - 'एकमेवाद्वितीयम्'। इस जगत् में हमें उनके कितने भी बहुरूप क्यों न दिखाई देते हों परन्तु चूंकि वे एक ही हैं इसलिये उनके विभिन्न रूपों के बीच आदान-प्रदान होता है, जिसे 'यज्ञ' कहते हैं। इस तरीके से संसार चलता रहता है और अपनी-अपनी मानसिकता के अनुसार लोग अपने-अपने कर्मों में लगे रहते हैं। अब ज्यों ही व्यक्ति का कुछ आन्तरिक विकास होता है, तब उसे यह बोध होता है कि केवल यक्ष, प्रेत आदि की पूजा करना ही आवश्यक नहीं है, केवल अपने ऊपर केन्द्रित रहकर प्रयत्न करने की अपेक्षा उसका गुजारा तो अन्य तरीकों से भी चल सकता है। और तब व्यक्ति घोर स्वार्थ से हटकर कुछ निःस्वार्थ कार्य करने लगता है और, इस प्रकार, वह भूतों और यक्षों की पूजा करने की अपेक्षा गंधर्वो और छोटे देवताओं की पूजा करने लगता है और तब वह पाता है कि उसका काम तो पहले की अपेक्षा और भी अधिक अच्छे तरीके से चल रहा है। इससे भी आगे यदि व्यक्ति को विश्वास आ जाए कि इस सब प्रयास के बिना भी उसका काम चल सकता है और वह अपना समय परमात्मा का ध्यान करने में लगा सकता है तो फिर स्वतः हो उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। प्रकृति का ऐसा ही विधान है। इस तरह आरोहण करते-करते जब व्यक्ति परमात्मा के संपर्क में आ जाता है तब फिर उसके ऊपर कोई बाहरी विधान लागू नहीं होता क्योंकि फिर वह परम् में चला जाता है और अपनी आत्मसत्ता में निवास करने लगता है। तब फिर वह सहज रूप से जो कोई भी कर्म करता है वह आनन्द के लिए ही करता है और किसी भी प्रकार के कर्मों को करने की उसकी कोई बाध्यता नहीं रहती, और सहज रूप से उसे जैसी प्रेरणा होती है उसके लिए सहज ही वैसी विशाल व्यवस्था होती जाती है क्योंकि उसके सारे कर्म तो उसके प्रभु के ही निमित्त होते हैं।
हमारे ऋषि मनुष्य के जीवन को 'यज्ञ का आरोहण' बताते हैं जो कि तामसिक, राजसिक और सात्त्विक प्रकार का होता है। पर तीनों ही जंजीरें हैं। आरोहण में मनुष्य को इन्हीं के द्वारा होकर चलना होता है।
परंतु सात्त्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों ही स्थितियाँ अपने शुद्ध रूप में नहीं मिलतीं। किसी एक तत्त्व की प्रधानता होने पर भी दूसरे दोनों तत्त्व भी न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहते ही हैं क्योंकि मनुष्य में केवल मन या बुद्धि ही नहीं अपितु प्राण और शरीर भी होते हैं इसलिए इनका भी अपना प्रभाव रहता ही है। इसलिए गीता जिस विशुद्ध रूप से सात्त्विक मनुष्य की बात करती है वह तो विरला ही होता है। परंतु ऐसा होने पर भी वास्तव में तो व्यक्ति बंधनमुक्त नहीं हो सकता। वह तो एक अन्य तत्त्व है जो कि किसी चाण्डाल में भी सक्रिय हो जाए, जगाई-मधाई जैसे किसी घोर पापी, अनाचारी में भी सक्रिय हो जाए तो तुरंत ही उसे पवित्र बना देता है। वह व्यक्ति तो प्रभु के चरणों में निवेदित हो जाता है और उनसे जुड़ जाता है। क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त अन्य कुछ तो सत्य है ही नहीं, बाकी सब तो केवल दिखावा मात्र ही है। गीता, भागवत् और सारे शास्त्रों में इसी बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति कहीं पर भी, कैसी भी स्थिति में क्यों न हो परन्तु जिस दिन उसके यह बात समझ में आ गई कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी मूल्यवान् नहीं है, सब निरर्थक है, उसी दिन से उसके जीवन में दूसरी धारा आरम्भ हो जाएगी, इससे पहले शुरू नहीं हो सकती।
परन्तु अपने सामान्य प्रगति क्रम में प्रकृति तामसिकता से राजसिकता की ओर और फिर सात्त्विकता की ओर गति करती है। हालाँकि एकाएक भी इनमें से निकल कर निस्त्रैगुण्य तक जाया जा सकता है। सात्त्विक व्यक्ति के लिए यह अधिक आसान है, और दूसरों के लिए अपेक्षाकृत कठिन है। परंतु फिर भी कोई बाध्यता नहीं है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की अन्तरात्मा कितनी विकसित हो चुकी है। पहुँचाएँगे। इसी प्रकार जब व्यक्ति को यह आभास हो जाता है कि सर्वत्र वह स्वयं ही मौजूद है तब तो सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति हर एक को इतना प्यार करता है जितना कि किसी माँ को अपने इकलौते बच्चे से भी न होता होगा। वह स्थिति ही दूसरी है। ऐसा व्यक्ति किसी की भलाई करने की सोचता ही नहीं क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, वह स्वयं ही सभी में मौजूद है। और इसी कारण उसे अपने ही सभी रूपों में प्रत्येक की वास्तविक आवश्यकता का भी भान होता है। इस चेतना के बिना तो व्यक्ति अपने ही विचारों के अनुसार, जिन चीजों की उसे स्वयं को चाह रहती है या फिर जो चीजें उसे स्वयं को पसंद हैं, उन्हीं के द्वारा दूसरों की भलाई करने की सोचता है कि वे चीजें दूसरे को भी प्राप्त हो जाएँ। अधिकांश व्यक्ति तो केवल भौतिक वस्तुओं के द्वारा ही भलाई करने की सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति तो बहुत ही कम होते हैं जो वास्तव में मनोवैज्ञानिक रूप से, या फिर कुछ आंतरिक रूप से भलाई करने की सोचते हैं। यह तो मनुष्य का अहं है जिसे लगता है कि वह किसी की भलाई कर सकता है। परन्तु जब वह दूसरी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को सभी से तादात्म्य महसूस होता है, उस स्थिति में उसे न केवल मनुष्यों से बल्कि पेड़-पौधों से, पशु-पक्षियों से भी प्रेम हो जाता है। और इस चेतना में वह किसी के साथ कोई अनुचित व्यवहार कर ही नहीं सकता। अवश्य ही इसका यह अर्थ नहीं है कि जहाँ तथाकथित अप्रिय व्यवहार की आवश्यकता हो वहाँ वह वैसा करने से चूकेगा। जब, जहाँ, जैसा व्यवहार अपेक्षित होगा वह ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। इसीलिए पश्चिम के मानवतावाद में, परोपकारिता में और भारतीय संस्कृति के 'सर्वभूत हिते रताः' में दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है।
अतः अपना और दूसरों का वास्तविक कल्याण तभी हो सकता है जब हम परमात्मा की ओर चलें, क्योंकि केवल वे ही जानते हैं कि किस व्यक्ति का भला कैसे हो सकता है। यदि वस्तुओं पर, या धन तथा अन्य किसी चीज पर ही कल्याण निर्भर होता तो परमात्मा सभी को समान रूप से स्वयं ही इन सब की आपूर्ति कर देते। परंतु वे हमारे मानदंडों के द्वारा कार्य नहीं करते। और वे फिर स्वयं अपने साथ ही तो यह सब व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए सच्ची भलाई तब होती है जब हम परमात्मा से जुड़े हों, क्योंकि तब हम वही काम करेंगे जो परमात्मा स्वयं अपने साथ कराना चाहेंगे और इसी में सच्ची भलाई है। बाकी सब तो मनुष्य का अहं है, भ्रम है।
प्रश्न : यदि व्यक्ति की भावना और सोच अच्छी हो, क्या तभी वह ऊपर की ओर उठ सकता है?
उत्तर : भावना तभी अच्छी होती है जब व्यक्ति का चैत्य पुरुष, उसकी अंतरात्मा कुछ विकसित होते हैं। अन्यथा तो व्यक्ति इतने घोर अहं में होता है कि दूसरों के बारे में सोच ही नहीं सकता। व्यक्ति के मन में दूसरे की पीड़ा के प्रति सहानुभूति, पशुओं के प्रति दया, अपने देश की दुर्दशा के प्रति पीड़ा आदि के भाव तभी होते हैं जब उसकी आत्मा कुछ विकसित होती है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति की भावना अच्छी होने पर भी उसे वास्तव में इसकी कोई समझ हो। परंतु चूंकि उसके अन्दर से यह भाव प्रकट हो रहा है इसलिए यह इस बात का संकेत है कि वह व्यक्ति सात्त्विक है। और सात्त्विक प्रकृति वाला व्यक्ति आगे जा सकता है, हालाँकि ऐसा होना आसान नहीं है। क्योंकि सात्त्विकता के बंधनों से छूट पाना, इन भावों से छूट पाना कि 'मैं परोपकारी हूँ, निर्लेप हूँ, मुझे कोई प्रतिफल नहीं चाहिए' बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य को अधिकांशतः तो यह आभास ही नहीं होता कि वह बंधन में है। इसके लिए तो व्यक्ति को परमात्मा से ही जुड़ना पड़ेगा। तभी वह इस बंधन से भी छूट सकता है। और जैसा गीता कहती है कि चूंकि सात्त्विक व्यक्ति की भीतर से अधिक तैयारी हो चुकी होती है इसीलिए तामसिक और राजसिक की अपेक्षा उसके लिए ऊपर उठना आसान होता है।
और जो इस बंधन से छूट निकलता है उसके लिए फिर भलाई-बुराई, परोपकार आदि के सभी मानदंड सतही हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा ने यह सारा ब्रह्माण्ड अपने आनंद के लिए रचा है, इसलिए उस व्यक्ति के लिए करने का काम यह होता है कि पहले इस रचना को समझे और इसके आनंद में स्वयं आनंदित हो। पृथ्वी पर जिन्होंने भी महत् कार्य किये हैं, जिन्होंने भी पृथ्वी के विकासक्रम में सहायता प्रदान की है, वे वे ही आत्माएँ या सत्पुरुष हैं जो परमात्मा से जुड़े हैं।
परन्तु व्यक्ति अज्ञान से आरंभ करता है और बहुत काल तक अज्ञान में ही लगा रहता है। अतिशय रूप से अपने-आप के विषय में ही सचेत रहने के कारण वह अहंकार को ही जीवन के मूल कारण और उसके संपूर्ण अर्थ के रूप में देखता है, न कि भगवान् को। वह स्वयं को कर्मों के कर्ता के रूप में देखता है और यह नहीं देख पाता कि जगत् के सारे कर्म, जिनमें उसके अपने आंतर और बाह्य सब कर्म भी सम्मिलित हैं, एक ही विश्व-प्रकृति द्वारा होनेवाले कर्म हैं, और अलग कुछ नहीं। वह अपने-आपको ही सब कमाँ का भोक्ता समझता है और यह कल्पना करता है कि सब कुछ उसी के लिए है, और इसलिए प्रकृति को उसे ही संतुष्ट करना चाहिए और उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं की अनुपालना करनी चाहिए; उसे यह नहीं सूझता कि प्रकृति को ऐसा कोई सरोकार नहीं कि उसे संतुष्ट करे और उसकी इच्छा की उसे कुछ भी परवाह नहीं है, अपितु प्रकृति तो एक उच्चतर वैश्व-संकल्प की आज्ञा का पालन करती है और उस देव को तृप्त करना चाहती है जो उससे, उसके कमाँ और उसकी सृष्टियों से अतीत है। मनुष्य की परिसीमित सत्ता, उसकी इच्छा और उसकी तृतियाँ उसकी अपनी नहीं, अपितु प्रकृति की हैं और प्रकृति इन सब चीजों को प्रतिक्षण उन भगवान् को यज्ञ-रूप से अर्पण किया करती है जिनके हेतु को सिद्ध करने के लिए वह इन सब चीजों को अज्ञात, अप्रकट साधनमात्र बनाती है। इस अज्ञान के कारण ही, जिसकी कि छाप अहंकार है, जीव यज्ञ के विधान की उपेक्षा करता है और संसार में जितना हो सकता है उतना सब कुछ अपने लिए ही बटोरना चाहता है और केवल उतना ही देता है जितना प्रकृति अपने भीतरी और बाहरी दबाव के द्वारा उसे देने को बाध्य करती है। यथार्थ में वह उससे अधिक कुछ नहीं ले सकता, जितना प्रकृति उसे उसके भाग के रूप में प्राप्त करने देती है, जितना प्रकृति में स्थित ईश्वरीय शक्तियाँ उसकी कामना पूरी करने के लिए देती हैं। यज्ञमय संसार में अहंकारविमूढ़ जीव मानो ऐसा है जैसे कोई चोर या लुटेरा हो जो इन दैवी शक्तियों का दिया हुआ सब कुछ लेता तो है, पर बदले में कुछ देने की नीयत नहीं रखता। वह जीवन के वास्तविक अभिप्राय से वंचित रह जाता है और चूंकि वह अपने जीवन तथा कर्मों का उपयोग यज्ञ के द्वारा अपनी सत्ता को उदार, विशाल और उन्नत बनाने में नहीं करता, इसलिए वह व्यर्थ ही जीता है।
इसमें कुछ बातें बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं परंतु इन्हें बार-बार देखने, समझने और पढ़ने के बावजूद भी प्रायः ही हम भूल जाते हैं। क्योंकि साधारणतया हम सदा ही अपने अहं में जीते हैं और सब समय उसे ही पोषित करते हैं। सभी समय हम अपने विचारों से, भले वे कितने भी उदात्त क्यों न हों, सम्मोहित रहते हैं। उदाहरण के लिये ये विचार कि मैं अमुक महान् कार्य करूँगा या फिर श्रीमाताजी के निमित्त काम करूंगा, उसके परिणामस्वरूप मेरी साधना होगी, आदि-आदि। इन्द्रियों के, मन के, बुद्धि के ये सभी क्रिया-कलाप सदा चलते रहते हैं और हम हमारे अहं के पोषण में लगे रहते हैं और हमें इस बात का कोई अंदेशा तक भी नहीं होता कि हम कोई गलती कर रहे हैं। क्योंकि हमें यह लगता हैं कि "मैं हूं' और 'मुझे' कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये। अच्छा वह है जो 'मेरे अनुकूल है और बुरा वह है जो 'मेरे' अनुकूल नहीं है। जो 'मेरे' व्यक्तित्व को महत्त्व देता है वह तो अच्छा है और जो नहीं देता वह बेकार है। ये सभी विचार हमारे अहं को ही परिपुष्ट करते हैं। सारे दिन यही चलता रहता है। श्रीअरविन्द यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अहंकार में लिप्त विमूढात्मा है।
वास्तव में तो केवल दो का ही अस्तित्व है: परम् पुरुष और उनकी आद्या शक्ति। परम् पुरुष ने स्वयं को इतने विभिन्न रूपों में प्रकट किया है और आद्याशक्ति उन रूपों में प्रविष्ट होकर परम् पुरुष के संकल्प को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक विचारों, भावनाओं, कर्मों आदि को उत्पन्न करती है और उन सब को उन असीम परमात्मा को भेंट करती है। इस सारी क्रियाकलाप में जो स्वयं को कर्त्ता मानता है और सभी कर्मों को अपने अहं पर अध्यारोपित करता है वह विमूढ़ है क्योंकि वास्तव में इस सब क्रियाकलाप में हमारा कोई लेन-देन नहीं होता। यह सब तो उन आद्याशक्ति या पराप्रकृति द्वारा किया जाता है और वे हमारी पसन्द नापसन्द से प्रभावित नहीं होतीं। हम देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ तथाकथित अच्छे कर्म करते हुए भी बुरे परिणाम घटते हैं और दूसरों को बुरे कर्म करते हुए भी तथाकथित अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। परंतु परा प्रकृति पर हमारे नैतिकता-अनैतिकता या सत्य या झूठ के मानदंड बाध्यकारी नहीं हैं। वह तो परम् प्रभु के संकल्प की अभिव्यक्ति के लिए जो आवश्यक है, वह कर्म करती है।
इसलिए गीता पहले तामसिक अवस्था का वर्णन करती है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने अहं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के दृष्टिकोण से देख ही नहीं पाता। वह हमेशा ही अहंपरक रूप से स्वयं की सुख-शांति के लिये और स्वयं को जो अच्छा लगे उसी अनुसार कर्म करना चाहता है, उसके अलावा नहीं। और फिर कर्म भी उसके स्वयं के लिए आवश्यक हो तो करना चाहता है, अन्यथा नहीं। हाँ, वह यह अवश्य चाहता है कि प्रकृति की कार्य-प्रणाली ऐसी हो कि उसे उसका वांछित सब कुछ मिल जाये – धन मिल जाये, मकान मिल जाये, समृद्धि मिल जाये, बहुत से प्रेम करने वाले लोग मिल जायें जो उसके बारे में ऊँचे विचार रखते हों। यह यज्ञ की तामसिक अवस्था है और ऐसे व्यक्ति का जीवन वृथा है - मोषं पार्थ स जीवति। निन्यानबे प्रतिशत लोग तो इसी श्रेणी में आ जाते हैं। हो सकता है कि कुछ में कोई दूसरा अंश भी हो परन्तु अधिकांश में तो यही भाव प्रमुख होता है कि 'मैं' हूँ, और फिर इस 'मैं' के संबंध से सारा प्रपंच। कोई जो निरा पशुतुल्य और तामसिक है, वह केवल खाने-पीने पर तथा शरीर के सुख-भोग आदि पर ही अधिक केन्द्रित होता है, जो कोई राजसिक स्तर का है वह प्राणिक आदान-प्रदान में लगा रहता है, और जो सात्त्विक स्वभाव का है वह उचित-अनुचित के विचारों के अनुसार चलता है। परंतु फिर भी अधिकांशतः यही भाव होता है कि उसके अपने ही विचार परमोच्च हैं और सभी व्यवस्था उसी के अनुसार होनी चाहिये। इन तीनों ही प्रकृति के लोगों का झुकाव प्रायः केवल तामसिक उद्देश्यों की पूर्ति की ओर ही होता है। ये सभी हमेशा ही व्यक्ति के स्थूल भौतिक भाग की कामनाओं, आवेगों आदि की सेवा में ही लगे रहते हैं। उसी सेवा के लिये बुद्धि तत्पर रहती है, उसी की सेवा में प्राण रत रहता है, उसी की सेवा हृदय करता है। यह प्रथम स्तर है, जो कि बहुत ही निम्न कोटि का स्तर है परन्तु अधिकांशतः मनुष्य इससे ऊपर नहीं जाता। वह केवल अपने 'अहं' पर या 'स्व' पर केन्द्रित रहता है, अन्य किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता। मनुष्य के दूसरे भागों के द्वारा इस प्रवृत्ति को कुछ रंग दे दिये जाते हैं। बुद्धि अपने रंग दे देती है, हृदय अपना कुछ रंग दे देता है जिससे ऊपरी रूप से दिखने में वह इतना भौंडा न दिखे, परंतु वास्तव में तो यह 'स्व' केंद्रित प्रवृत्ति ही हावी रहती है। न्याय, नैतिकता आदि को तो व्यक्ति जब, जहाँ और जैसा अनुकूल हो उस अनुसार केवल इसी की पूर्ति के लिये उपयोग में लेता है। किसी दूसरे का आकलन करते समय व्यक्ति तुरन्त कह देता है कि उसका अमुक काम गलत है और नहीं किया जाना चाहिये परन्तु बात जब स्वयं की होती है तो उसी काम को सही और उचित ठहरा देता है। यज्ञ का यह तामसिक स्तर है। इस स्तर पर भ्रम का सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति सोचता है कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसके अहं की पूर्ति के लिये सारे काम हो रहे हैं और होने चाहिये। जबकि प्रकृति को इससे कोई लेना-देना नहीं है। उसके लिये तो सब परमात्मा के बहुरूप हैं और वह उन परमात्मा के संकल्प और उनके सत्य के अनुसार मन, प्राण, शरीर और आत्मा में उसी प्रकार के स्पंदन पैदा करती है। और ये सभी स्पंदन वह उन्हीं की प्रसन्नता के निमित्त करती है और उन्हें ही समर्पित करती है। उसका अन्य कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। और चूँकि वह परमात्मा की प्रसन्नता के ही निमित्त सब कुछ करती है इसलिए स्वतः ही उसके सारे कार्य उन्हें समर्पित होते हैं। जबकि हमने अपनी जो दुनिया बना रखी है वह इसके एकदम विपरीत है। हम उसी में फंसे रहते हैं इसीलिये अज्ञान में रहते हैं। हमारी इस संकीर्ण स्थिति में यदि कोई थोड़ी-सी अभीप्सा प्रवेश कर जाए, या कोई उदात्त विचार आ जाए तो कुछ छोटा-मोटा अनुभव हो जाता है और धीरे-धीरे यज्ञ की यह ऊर्ध्व प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परंतु अधिकतर मनुष्यजाति के लिये तो ये सारे आयाम बंद होते हैं। अधिकांश मनुष्यजाति के यज्ञ का यही स्तर होता है और ऐसी अवस्था वाला मनुष्य वृथा ही जीता है, 'मोघं पार्थ स जीवति'।
जब व्यक्ति अपने क्रिया-व्यवहारों में दूसरों में स्थित आत्मा के महत्त्व को उतना ही अनुभव करने और स्वीकार करने लगता है जितना कि वह अपने अहं की शक्ति और आवश्यकताओं को मानता है, जब वह अपने कार्यों के पीछे विश्वप्रकृति को अनुभव करने लगता और विश्वदेवताओं के द्वारा उस एक अखण्ड और अनन्त की झलक पाता है, केवल तभी वह अहं द्वारा निर्धारित सीमाओं के अतिक्रमण और अपनी आत्मा के प्रकटीकरण के मार्ग पर होता है। वह एक ऐसे धर्म-विधान को जानना आरंभ करता है जो उसकी कामनाओं के विधान से भिन्न हो, जिसके प्रति उसकी कामनाओं को अधिकाधिक अधीनस्थ और आश्रित होना होगा: अब वह निरी अहंकारमय सत्ता की जगह एक उदार और नैतिक सत्ता में विकसित हो जाता है। अब वह दूसरों में निहित आत्मा की माँग को अधिक महत्त्व देने लगता है और स्वयं अपने अहं के दावों को कम महत्त्व देता है, वह अहंकार और परहित भाव के बीच के संघर्ष को स्वीकार करता है और अपनी परोपकारवृत्ति को बढ़ाकर अपनी चेतना और सत्ता का विस्तार करता है। वह प्रकृति और प्रकृति में स्थित दिव्य शक्तियों का बोध करने लगता है जिनके प्रति उसे यजन, अर्चन और अनुपालन उत्सर्ग करने हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा और इन्हीं के विधान के द्वारा मानसिक और भौतिक दोनों जगतों की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, और वह यह जान जाता है कि केवल उन्हीं की उपस्थिति और महत्ता को अपने विचार, संकल्प और प्राण में संवर्धित करने से वह अपनी शक्ति, ज्ञान और उचित कर्म को तथा इनसे प्राप्त होनेवाली तुष्टि-पुष्टि को बढ़ा सकता है। इस प्रकार वह जीवन के जड़भौतिक और अहंपरक भाव में धार्मिक और अतिभौतिक भाव को जोड़ देता है और अपने-आप को सीमित से होकर अनन्त में ऊपर उठने के लिए तैयार करता है।
जब व्यक्ति का कुछ विकास होता है, उसकी मानसिकता का मनोविज्ञान का, उसके हृदय का कुछ विकास होता है तब उसे लगता है कि जीवन में केवल स्वयं के बारे में, अपनी ही पसंद-नापसंद, अपने सुख-दुःख के बारे में सोचने और केवल अपने ऊपर ही केन्द्रित रहने के अतिरिक्त भी कुछ है। सारी व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिये इसके ऊपर एक नैतिक विधान भी है। और यदि उस विधान में कहीं कोई भंग पड़ता है तो व्यवस्था चलेगी नहीं। इसलिये सही रूप से काम चलता रहे उसके लिए किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना आवश्यक है, चीजों के बीच में किस प्रकार का आपसी तालमेल है, किस प्रकार का संतुलन है, यह सब भान होने लगता है। और इसी को अलग-अलग देवताओं के साथ आदान-प्रदान होना कहते हैं। हालाँकि व्यक्ति ऐसा सोच कर और सचेतन रूप से नहीं करता कि वह देवताओं के साथ व्यवहार या आदान-प्रदान कर रहा है। ऐसा तो विचार ही नहीं आता क्योंकि उसे इस बात का भान नहीं होता कि देवताओं का भी कोई अस्तित्व है। पर बिना सोचे-समझे भी व्यक्ति धीरे-धीरे केवल स्वयं के क्षुद्र स्वार्थ की अपेक्षा समाज के विधानों को भी महत्त्व देने लगता है। वह यह भी सोचने लगता है कि उसके कृत्य से दूसरों को कैसा महसूस होगा। उसके कारण किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिये। वह इन सब चीजों का महत्त्व समझने लगता है। उसे यह समझ में आ जाता है कि अन्य सभी के हित में ही उसका भी हित साधन है और अनैतिक व्यवहार करने में स्वयं उसे ही तकलीफ होगी। यह बात बहुत अधिक सोच-विचार कर नहीं अपितु सहज रूप से ही कुछ परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पर समझ में आने लग जाती है। यह दूसरा स्तर है, जिसमें आदान-प्रदान पहले से बेहतर होने लगता है। यह मध्यमा गति है। इसे राजसिक स्तर भी कह सकते हैं जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे अच्छा व्यवहार तभी प्राप्त होगा जब वह स्वयं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इस स्तर पर विभिन्न श्रेणी के लोग हो सकते हैं। राजसिक होकर भी कोई व्यक्ति तामसिक अवस्था के अधिक निकट हो सकता है और कोई अधिक सुसंस्कृत हो सकता है और संभव है कि सब बातों के बावजूद वह कुछ आंतरिक रूप से भी खुला हो और परमात्मा को भी कुछ महसूस करता हो। इसमें कोई तय नियम नहीं है। व्यक्ति तामसिक अवस्था में होकर भी परमात्मा को महसूस कर सकता है। इसलिए किसी भी अवस्था पर यह संभव है कि व्यक्ति परमात्मा को महसूस करे। परमात्मा कभी भी, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति में प्रकाशित हो सकते हैं, वह तो एक भिन्न क्रिया है। परंतु सामान्यतया व्यक्ति में ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे भीतर का प्रकाश बढ़ता है त्यों-ही-त्यों वह इस प्रकार क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। यह है यज्ञ का आरोहण ।
परन्तु यह केवल एक सुदीर्घ मध्यवर्ती अवस्था है। यह अवस्था अभी भी कामना के विधान के अधीन होती है, सभी चीजों का केंद्र उसके अहंकार के दृष्टिकोण और आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है, तथा उसकी सत्ता और उसके कर्मों का नियंत्रण प्रकृति के द्वारा होता है, यद्यपि यह कामना एक संयत और मर्यादित कामना ही होती है, एक परिष्कृत अहंकार और एक ऐसी प्रकृति होती है जो कि प्रकृति के उच्चतम तत्त्व, सात्त्विक तत्त्वत, द्वारा अधिकाधिक सूक्ष्म और प्रकाशित कर दी जाती है। यह सब अभी भी क्षर, सीमित और व्यष्टिगत के क्षेत्र के अंतर्गत ही रहता है, भले यह एक बहुत अधिक विशाल क्षेत्र हो। सच्चा आत्मज्ञान और फलतः सच्चा कर्ममार्ग इसके परे है; क्योंकि ज्ञानयुक्त होकर किया जानेवाला यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वही पूर्ण कर्म को लाता है। यह अवस्था तभी आ सकती है जब मनुष्य यह अनुभव करे कि उसके अन्दर की आत्मा और दूसरों के अन्दर जो आत्मा है वे एक ही सत्ता हैं और यह आत्मा अहंकार से कुछ उच्चतर वस्तु है, यह एक अनन्त, नैर्व्यक्तिक, विश्वव्यापी सत् है जिसमें सब प्राणी गति करते हैं और अपना अस्तित्व धारण रखते हैं, - जब वह यह बोध करता है कि समस्त विश्व-देवता जिनके प्रति वह अपने यज्ञ भेंट करता है, वे एक ही अनन्त परमेश्वर के अनेक रूप हैं और जब वह उस एक परमेश्वर-सम्बन्धी अपनी सीमित और सीमाबद्ध करनेवाली धारणाओं का परित्याग कर के उन्हें एक अनिर्वचनीय परमदेव जानता है जो एक ही साथ सीमित और अनन्त हैं, जो एक पुरुष हैं और साथ ही अनेक भी, जो प्रकृति के परे होकर भी प्रकृति के द्वारा अपने-आपको प्रकट करते हैं, जो गुणों के बंधनों के परे होकर भी अपने अनन्त गुणों के द्वारा अपनी सत्ता की शक्ति को निरूपित किया करते हैं। इन्हीं पुरुषोत्तम को यज्ञ समर्पित करना होता है, किसी क्षणिक वैयक्तिक कर्मफल के लिए नहीं, अपितु जीव द्वारा भगवान् को प्राप्त किये जाने के लिए और इसलिए कि भगवान् के साथ समस्वरता और एकता में रहा जा सके।
ज्यों-ज्यों व्यक्ति का विकास होता है त्यों-त्यों उसके नैतिकता के बोध भी और अधिक परिष्कृत होते जाते हैं और वह उनके अनुसार जीना शुरू कर देता है। अमुक काम करते समय कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो भी वह उसके लिये तैयार रहता है। उसके भीतर ऐसी चीज विकसित हो जाती है जिसे बाहरी नुकसान की अपेक्षा नैतिक विधान में भंग होना ज्यादा नुकसानदायक महसूस होता है क्योंकि उसे अब उसमें आनन्द प्राप्त होता है। बिना आनन्द के तो यज्ञ का आरोहण हो ही नहीं सकता।
धीरे-धीरे अब व्यक्ति अपने दुःख-दर्द से इतना प्रभावित नहीं होता जितना कि दूसरों के दुःख-दर्द से होता है। उसमें संवेदनाएँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वह दूसरों का दुःख-दर्द देख ही नहीं पाता। ये सब बातें सहज रूप से व्यक्ति के भीतर होना प्रारम्भ हो जाती हैं। उसके भीतर कोई चीज ऐसी होती है जो इस बात को महसूस करती है कि दूसरे के अंदर वही चीज है जो उसके स्वयं के भीतर है और यदि उसके कारण दूसरों को तकलीफ होती है तो अंततः उसे भी तकलीफ होगी। जब व्यक्ति आरोहण मार्ग पर होता है तब वह इन सब बातों के विषय में बिना सोचे-समझे भी सहज रूप से दूसरों की तकलीफ-आराम के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। उसमें एक ऐसा भाग विकसित हो जाता है जो अपने ही अहं की तुष्टि को, अपने ही मन, प्राण और शरीर की तुष्टि को अधिक महत्त्व न देकर दूसरों के बारे में भी संवेदनाएँ-भावनाएँ रखता है। उसमें आनन्द का एक अधिक गहरा स्रोत खुल जाता है और वह एक अधिक ऊँचे स्तर पर आ जाता है जहाँ वह एकत्व को महसूस कर सके। साथ ही उसमें यह भाव भी विकसित हो सकता है कि भगवान् हैं। वे ही सबके मालिक हैं और सब शरीरों में वे ही विद्यमान हैं। ऐसा उसके परिवार, वातावरण, संस्कारों, संस्कृति आदि पर निर्भर करता है। परन्तु यह संवेदनशीलता आना मुख्य बात है और जब यह प्रास हो जाती है तब व्यक्ति एक अधिक उच्च स्थिति पर आ जाता है। इससे ऊपर की स्थिति तो योगियों की है जिसमें व्यक्ति को परमात्मा का, श्रीमाताजी का बोध हो जाता है और वह उन्हें समर्पित हो जाता है। फिर श्रीमाताजी ही उसकी सत्ता को अधिग्रहीत कर लेती हैं और वह उनके हाथों में एक यंत्र बन जाता है और श्रीमाँ उससे जो करवाना चाहती हैं वही करा लेती हैं। व्यक्ति का कोई अहमात्मक 'स्व' नहीं रह जाता। यह भाव प्राप्त होने पर वह फिर तीनों गुणों से परे चला जाता है अन्यथा तो वह सात्त्विक स्तर पर आकर ही रुक जाता है।
यज्ञ के आरोहण को हम अनेकों तरीकों से देख और समझ सकते हैं। यहाँ हमने उन अनेकों में से एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है जिसमें कि व्यक्ति अधिकाधिक संवेदनशील होता जाता है। व्यक्ति स्वयं के सुख-दुःख से अधिक दूसरों के सुख-दुःख के प्रति संवेदनशील हो जाता है। भरत जी के चरित्र का उदाहरण हम देखें कि किस प्रकार भगवान् श्रीराम की पीड़ा का विचार कर के उन्हें स्वयं इतनी गहरी पीड़ा का अनुभव हुआ और उन्होंने स्वयं अपना जीवन तपस्यामय बना दिया, इस सबका वर्णन तो हम रामायण में देख ही सकते हैं। यह आत्मा का भाव है। उसके प्रति खुले बिना तो इतना संवेदनशील होना संभव नहीं है। व्यक्ति जितना ही अधिक आत्मा के संपर्क में होगा, उसकी संवेदनशीलता उतनी ही बढ़ती जाएगी और वह स्थूल की बजाय अधिकाधिक सूक्ष्म चीजें अनुभव करने लगेगा, उनके प्रति संवेदनशील हो जाएगा।
गीता के यज्ञ-सिद्धांत का निरूपण दो पृथक् संदर्भों में हुआ है; एक हम तीसरे अध्याय में पाते हैं, दूसरा चौथे अध्याय में; पहला निरूपण ऐसी भाषा में है जिसे यदि अपने-आप में ही लिया जाए तो प्रतीत होता है कि गीता केवल आनुष्ठानिक यज्ञ की बात कह रही है, दूसरा निरूपण उसी की व्याख्या एक व्यापक दार्शनिक प्रतीकात्मक अर्थ में कर के एकाएक ही उसके संपूर्ण अभिप्राय को बदल देता है और उसे आंतरिक और आध्यात्मिक सत्य के एक ऊँचे क्षेत्र तक उठा ले जाता है... [यहाँ हमें] गीता की ही भाषा में यज्ञ के संबंध में एक पूर्णतः प्रत्यक्ष और विशद व्याख्या प्राप्त होती है जो कि शब्दों के प्रतीकात्मक प्रयोग के बारे में और गीता की शिक्षा के द्वारा प्रतिपादित यज्ञ के मनोवैज्ञानिक अथवा अध्यात्मपरक होने के विषय में बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं छोड़ती"...यज्ञ का यह विशद वर्णन ही यज्ञ की एक ऐसी विशाल और व्यापक व्याख्या देता हुआ चलता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गयी है कि यज्ञ की क्रिया, उसकी अग्नि, हवि, होता और भोक्ता, उस यज्ञ का ध्येय और उद्देश्य, सब कुछ एकमेव ब्रह्म ही है।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।। २४।।
२४. अर्पण-रूप क्रिया ब्रह्म है, घृत आदि पदार्थ ब्रह्म है, ब्रह्म-रूप अग्नि में ब्रह्म के द्वारा हवन होता है; उस ब्रह्मरूप कर्म में समाधि के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्तव्य लक्ष्य होता है।
तो यही वह ज्ञान है जिससे युक्त होकर मुक्त पुरुष को यज्ञकर्म करना होता है। इसी ज्ञान की घोषणा प्राचीन काल में 'सोऽहं', 'सर्व खल्विदं ब्रह्म, ब्रह्म एव पुरुषः' आदि महान् वेदांतिक उक्तियों में हुई थी। यह समग्र एकत्व का ज्ञान है; यह वह 'एक' है जो कर्ता, कर्म और कर्मोद्देश्य के रूप में तथा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के रूप में अभिव्यक्त है। जिस विश्वशक्ति में कर्म की आहुति दी जाती है वह स्वयं भगवान् हैं; आहुति की उत्सर्ग की हुई शक्ति भगवान् हैं; जिस किसी वस्तु की आहुति दी जाती है वह भगवान् का ही कोई रूप होती है; आहुति देने वाले भी मनुष्य के अन्दर स्वयं भगवान् ही हैं, क्रिया, कर्म, यज्ञ सब गतिशील क्रियाशील भगवान् ही हैं; यज्ञ के द्वारा गन्तव्य स्थान भी भगवान् ही हैं। जिस मनुष्य को यह ज्ञान है और जो इसी ज्ञान में रहता और कर्म करता है उसके लिए कोई कर्म बंधनकारी नहीं हो सकते, उसका कोई कर्म वैयक्तिक और अहंकारमय रूप द्वारा हस्तगत नहीं होता। दिव्य पुरुष ही अपनी दिव्य प्रकृति के द्वारा अपनी सत्ता में कर्म करते हैं, अपनी आत्म-चेतन विश्व-शक्ति की अग्नि में सब कुछ की आहुति देते हैं; और इस सब भागवत्-परिचालित गति और कर्म का लक्ष्य होता है भगवान् के साथ युक्त जीव द्वारा भगवान् की दिव्य सत्ता और चेतना के ज्ञान को प्राप्त करना और उसे अधिकृत करना। इसे जानना, इसी एकत्व-साधने वाली चेतना में निवास करना और उसी में कर्म करना ही मुक्त होना है।
परन्तु योगियों में भी सभी ने इस ज्ञान को नहीं प्राप्त किया है।
गीता तीसरे अध्याय में यज्ञ के बारे में जो कह रही थी उसे तो भ्रमवश बाहरी अर्थात् केवल आनुष्ठानिक यज्ञ के अर्थ में लिया भी जा सकता है, और अधिकांश लोग लेते भी उसी अर्थ में हैं, परन्तु यहाँ चौथे अध्याय में यज्ञ के विषय में गीता जो कह रही है उससे तो कोई संदेह ही नहीं रह जाता कि गीता का यज्ञ मात्र बाह्य आनुष्ठानिक यज्ञ नहीं है। गीता उसे मनोवैज्ञानिक और आंतरिक धरातल तक उठा ले जाती है और वहाँ उसका निरूपण करती है। अगर इस आंतरिक मनोवैज्ञानिक अर्थ का निरूपण न हुआ होता तो वेदों के ही समान गीता के प्रति भी यह मिथ्या-धारणा दृढ़ हो जाती कि गीता केवल बाह्य अनुष्ठान का ही प्रतिपादन कर रही है और उसका कोई आंतरिक अर्थ नहीं है। यहाँ गीता के अनुसार जब व्यक्ति ब्रह्म भाव में आ जाता है और उस भाव में कर्म करता है तो उसके कर्म प्रभु की प्रकृति से ही चालित होते हैं और उनकी ओर ही जा रहे होते हैं। वह उनसे बद्ध नहीं होता। जब व्यक्ति को अहं का कोई भान ही नहीं है और सभी कुछ ब्रह्मरूप देखता है और परमात्मा को ही कार्यरत देखता है तब वह मुक्त हो जाता है।
------------------------------------------------------
"प्राचीन वैदिक पद्धति में सदा ही एक दोहरा अर्थ रहा है, भौतिक तथा दूसरा मनोवैज्ञानिक, बाह्य तथा रूपकात्मक, यज्ञ का बाह्य अनुष्ठान तथा उसकी सब विधियों का आंतरिक आशय। परन्तु प्राचीन वैदिक गुह्मवादियों (ऋषियों) की गूढ़ रूपकात्मक भाषा को, जो सर्वथा सटीक, अद्भुत, कवित्वमय और मनोवैज्ञानिक अथवा अध्यात्मपरक थी, गीता के काल से बहुत पूर्व ही लोग भूल चुके थे, और गीता में उसी के स्थान पर वेदांत और पश्चात्-कालीन योग के भाव को लेकर व्यापक, सर्वसामान्य और दार्शनिक भाषा का प्रयोग किया गया है। यज्ञाग्नि कोई भौतिक अग्नि नहीं अपितु ब्रह्माग्नि है अथवा यह ब्रह्म की ओर जानेवाली ऊर्जा, आंतरिक अग्नि, यज्ञ के पुरोहित-स्वरूप अंतःशक्ति है जिसमें आहुति दी जाती है; अग्नि है आत्म-संयम या शुद्धिकृत इन्द्रिय-क्रिया अथवा राजयोग और हठयोग में समान रूप से प्रयुक्त श्वास-प्रश्वास के नियमन की (प्राणायाम-साधना की) प्राणशक्ति है, अथवा अग्नि है आत्म-ज्ञानाग्नि, आत्मार्पणरूप परम यज्ञ को अग्निशिखा। यज्ञ से बचे हुए भाग का भोजन करना अमृत बताया गया है; और यहाँ हम अब भी उस प्राचीन वैदिक प्रतीकवाद का कुछ अंश पाते हैं जिसमें सोमरस को अमृत का भौतिक प्रतीक कहा जाता था - अमृत वह दिव्य परमानन्द का अमरत्व प्रदान करने वाला हर्ष-आनन्द है जो यज्ञ से प्राप्त होता, देवताओं को चढ़ाया जाता और मनुष्यों द्वारा पान किया जाता है।
परन्तु गीता कहती है कि अधिकतर योगियों को भी यह चीज नहीं प्राप्त होती। यह तो किसी बहुत ही लम्बी साधना के द्वारा या फिर अकस्मात् हुई भगवत्-कृपा से ही संभव है। अन्यथा यह चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। हो सकता है कि हमें सैद्धांतिक रूप से, विचार रूप में यह बात समझ में आ जाए, इसका विश्वास हो जाए, इसका बोध हो जाए कि चूंकि हमारे गुरु यह बात कह रहे हैं या फिर चूँकि गीता कह रही है तो यह बात पूरी तरह सत्य है, परन्तु वह केवल एक मानसिक विचार हो होगा और हमारे लिए वह एक जीवंत अनुभव नहीं होगा। उसे हम अपनी प्राणिक और भौतिक प्रकृति पर अंकित नहीं कर सकते। हमारे अवचेतन भागों में भिन्न-भिन्न तरीके की स्थूल गतियाँ यांत्रिक रूप से अपरिवर्तित ही चलती रहती हैं। इस विचार से हमारा केवल थोड़ा उत्थान थोड़ा परिष्करण होता है और हम कुछ संवेदनशील बन जाते हैं। जैसे ही हमारे दैनन्दिन कार्यकलापों के दौरान हमें थोड़ा-सा भी विचार करने का मौका मिलता है वैसे ही हम पुनः सचेत हो जाते हैं कि हम स्व-केन्द्रित हो रहे हैं। परन्तु इस बात की अनुभूति और स्पष्ट बोध कि सब में ब्रहा हो व्याप्त हैं और सभी कुछ ब्रह्मस्वरूप ही है, बहुत ही मुश्किल है। यह अनुभूति तो योगियों को भी आसानी से नहीं होती, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यदि हम सब में ब्रह्म का दर्शन कर सकें, यह अनुभव कर सकें कि हमारे भीतर की आत्मा और दूसरों के भीतर की आत्मा एक ही है, और उस चेतना में, दिव्य प्रकृति में निवास कर सकें तब फिर वह दिव्य प्रकृति जो भी कर्म करवायेगी, जो भी भाव लायेगी, जो भी विचार लायेगी हम उन सभी में सदा ही आनन्दित रहेंगे। उनमें कर्म से हमारी कोई लिप्तता अथवा बाध्यता होगी ही नहीं क्योंकि हम तो उन सब से ऊपर होंगे और उनको होता देख रहे होंगे। इस कारण उनका कोई कार्य-कारण प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए दिव्य कर्मी को 'सर्वारंभ परित्यागी' अर्थात् सभी आरम्भों के त्यागी की संज्ञा दी जाती है। वह किसी कार्य का आरम्भ नहीं करता। उसकी कोई स्वतंत्र व्यक्तिगत इच्छा रहती ही नहीं। हमारे कर्म फिर दिव्य प्रकृति से ही चालित होंगे। जिस समय जैसी आवश्यकता होगी वैसा विचार आ जाएगा, वैसा ही कर्म हो जायेगा। इसलिये जब कर्मों का कर्त्ता वह स्वयं नहीं रहता तो फिर मानसिकता में कर्म-जनित कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होती। उसकी सत्ता पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति खुली होती है और उन्हें समर्पित होती है और वह स्वयं को ब्रह्मस्वरूप जान लेता है। परन्तु गीता इसका वर्णन करने के बाद कहती है कि यह स्थिति योगियों को भी दुर्लभ है। और यदि मानसिक रूप से हम इसे समझ भी लें तो भी यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। परंतु धीरे-धीरे मन में यह विचार दृढ़ हो जाएगा, और फिर यह भावनाओं में आने लगेगा, जब भी हमें थोड़ा-सा विचार करने का मौका मिलेगा वैसे ही हम अधिक सजग होने लगेंगे और हम उस दृष्टिकोण से काम करने लगेंगे। परन्तु उस दृष्टिकोण से काम करना अलग बात है और जीवंत रूप से ब्रह्म को महसूस करना और देखना अलग बात है। यह तो मात्र एक मानसिक समझ ही है कि सबमें एक ही ब्रह्म विद्यमान है, केवल श्रीमाताजी व श्रीअरविन्द ही हमारे आराध्य हैं और उनके अलावा और किसी की सत्ता नहीं है और हमें इस बात में जरा भी संशय नहीं है, हमारा दिल और दिमाग भी यही बात कहता है परंतु फिर भी जीवंत रूप से हमें इसका अनुभव हो यह आवश्यक नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे अवचेतन भाग अपना प्रभाव डालते रहते हैं और अपनी यांत्रिक क्रियाएँ चालू रखते हैं, मनस् अपनी तय धुन के अनुसार उसी ढर्रे पर चलता रहता है, इंद्रियाँ अपने ही चक्करों में फंसी रहती हैं। जब परमात्मा से, श्रीमाताजी व श्रीअरविन्द से जुड़ने के बाद कुछ ऊर्जा व शक्ति हमें प्राप्त होती भी है उसे भी ये भाग यथासंभव छितरा देते हैं, विकृत कर देते हैं और उसे निष्प्रभावी बना देते हैं। जैसे ही साधक को कुछ शक्ति प्राप्त होती है वैसे ही उसमें दूसरों के कल्याण के विचार, दूसरों की सहायता करने के अहंपरक विचार, या फिर उस शक्ति को बिखेरने के अन्य कोई विचार आए बिना नहीं रह सकते। इस दुष्चक्र को तोड़ना परम् आवश्यक है और इसके पीछे निरर्थक शक्ति व्यय करने से बेहतर तरीका है कि जब हमें दिल-दिमाग में सद्गुरु के प्रति, श्रीमाताजी व श्रीअरविन्द के प्रति पूरा विश्वास आ गया है तो फिर जैसे ही मौका मिले वैसे ही हमें उनसे निवेदन करना चाहिये। यह भाव तो होता ही है कि 'उनकी जैसी इच्छा हो उस रूप से वे हमें काम में लें' परंतु साथ ही हम अपनी सभी क्रियाओं को उनके समक्ष रख दें और जो क्रियाएँ और चीजें हमसे संयमित नहीं हो रही हैं उनके लिए उनसे निवेदन करें कि वे उन्हें अतिक्रम करने में हमारी सहायता करें। यह निवेदन करें कि 'मेरी शक्ति इधर-उधर बिखर रही है जबकि वह सारी शक्ति आप ही को समर्पित होनी चाहिये। तो हम देखेंगे कि हम इस मार्ग पर आगे बढ़ने लग जाएँगे। यह एक व्यावहारिक तरीका है। हालाँकि हमारे हृदय में और दिमाग में पूर्ण विश्वास होता है परन्तु प्राण में, संवेदनों में, भौतिक शरीर में ऐसा नहीं होता। वह तो तब होगा जब श्रीमाताजी की शक्ति ऊपर से अवचेतन में, भौतिक शरीर में और बाहरी करणों में प्रवेश करेगी, उनमें अवतरित होगी। और इसमें समय लगता है। इसका श्रीअरविन्द ने अपनी पुस्तकों में खूब वर्णन कर ही रखा है। हो सकता है कि अचानक ऐसा भाव आ जाये और हमें यह अनुभव हो जाये कि सब जगह केवल श्रीमाताजी ही विराजमान हैं। ये सभी चीजें हमें और अधिक तैयार करती हैं। ये हमारे संवेदनों पर, प्राण पर, हमारी क्रियात्मक प्रकृति पर प्रभाव डालती हैं और इस प्रकार के बार-बार होते अनुभवों को सहायता से मनुष्य मार्ग पर चलता जाता है। परंतु केवल किसी एक बोध से ही सारा काम हो जाता तो फिर तो सब बहुत आसान हो जाता।
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ।। २५।।
२५. कुछ योगीजन केवल देवताओं के निमित्त यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं; और अन्य (योगीजन) ब्रह्म-रूप अग्नि में स्वयं यज्ञ के ही द्वारा यज्ञ करते हैं, (अर्पण करते हैं)।
दैव यज्ञ करनेवाले भगवान् की धारणा अनेक रूपों और शक्तियों में करते हैं और विविध साधनों, धर्मों, विधानों के द्वारा, अर्थात् कह सकते हैं कि, कर्मसंबंधी सुनिश्चित विधि-विधान, आत्म-संयम और समर्पित कर्म के द्वारा उन्हें ढूँढ़ते हैं; और जो ब्रह्माग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करनेवाले ज्ञानी हैं उनके लिये, यज्ञ का भाव है कि जो कुछ कर्म करें उसे सीधे स्वयं भगवान् को अर्पण करना, अपनी सभी क्रियाओं को एकीभूत भागवत् चेतना और शक्ति में निक्षिप्त कर देना ही एकमात्र साधन है, एकमात्र धर्म है। यज्ञ के साधन विविध हैं; हव्य भी नानाविध हैं।
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ।। २६॥
२६. कुछ मनुष्य श्रोत्र आदि इन्द्रियों का संयम-रूप अग्नि में हवन करते हैं; दूसरे मनुष्य शब्द आदि विषयों का इन्द्रियरूप अग्नि में हवन करते हैं।
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ।। २७।।
२७. और अन्य कोई मनुष्य समस्त इन्द्रियों की क्रियाओं का और प्राण-शक्ति की क्रियाओं का ज्ञान से प्रदीप्त हुई आत्मसंयम-योग रूप अग्नि में हवन करते हैं।
एक आत्म-संयम और आत्म-अनुशासन रूपी आंतरिक अथवा मनोवैज्ञानिक यज्ञ है जिससे उच्चतर आत्मसंवरण (self-possession) तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है... अर्थात्, एक साधना यह है जिसमें इन्द्रियों के विषयों को ग्रहण तो किया जाता है, पर उस इन्द्रिय क्रिया-व्यवहार से मन को विक्षुब्ध या प्रभावित नहीं होने दिया जाता, इन्द्रियाँ स्वयं ही विशुद्ध यज्ञाग्नि बन जाती हैं। फिर यह भी एक साधना है जो इन्द्रियों को शांत-स्थिर कर देती है ताकि स्थिर और शांत मनःक्रिया के परदे के भीतर से अंतरात्मा अपनी विशुद्धता में प्रकट हो सके। एक साधना यह है जिससे, आत्मतत्त्व का बोध होने पर, इन्द्रिय-बोध के सभी कर्म और प्राण-सत्ता के सभी कर्म उस एक स्थिर प्रशांत आत्म-स्थिति में ही ग्रहण किये जाते हैं।
"इन्द्रियाँ स्वयं ही विशुद्ध यज्ञाग्नि बन जाती हैं" इससे यह अर्थ निकलता है कि इन्द्रियों को उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भी काम में लिया जा सकता है और निम्नतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भी। यदि हम उन्हें उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये काम में ले रहे हैं तो वे हमें ब्रह्म की ओर ले जायेंगी। इनका अनुशासित और विवेकपूर्ण उपयोग होना प्रारम्भ हो जायेगा और इनमें शांति आ जाएगी। यदि हम इन्द्रियों का उपयोग अपने प्राण तथा अहं आदि निम्नतर हेतुओं को पुष्ट करने के लिये करते हैं तो ये बहुत अशांत हो जाती हैं। यदि हम इन्हें उच्चतर हेतुओं के लिये ऊपर से निर्देशित करेंगे तो फिर ये शांत हो जायेंगी और हमारे भीतर और अधिक प्रकाश फैलेगा। हमारा यज्ञ अधिक अच्छी तरह होगा। फिर ये सभी इन्द्रियाँ परमात्मा का, हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जायेंगी जो इनके द्वारा देखती, सुनती और अनुभव करती है।
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संशितव्रताः ।। २८ ।।
२८. कुछ ऐसे हैं जो अपनी भौतिक संपदाओं को यज्ञ में भेंट कर देते हैं, दूसरे आत्मानुशासन की तपश्चर्याओं का हवन करते हैं, कुछ अन्य योग के किसी रूप (हठयोग, राजयोग आदि) का यज्ञ करते हैं, और दूसरे हैं जो तीक्ष्ण (कठोर) व्रतों से युक्त हो अपने अध्ययन और ज्ञान का यज्ञ करते हैं।
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।। २९।।
२९. कुछ दूसरे ऐसे हैं जो अपान वायु (भीतर आनेवाले श्वास में) प्राण (बाहर जानेवाले प्रश्वास) का और प्रश्वास में श्वास का हवन करते हैं और इस प्रकार प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणायाम के अभ्यास में तत्पर रहते हैं।
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।। ३०।।
३०. अन्य दूसरे मनुष्य अपने आहार को नियत और संयत कर के प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं; ये सभी यज्ञ के जानने वाले लोग यज्ञ के द्वारा अपने पापरूप मलों को दूर कर देते हैं ।
इन सब से फलतः सत्ता का शुद्धिकरण होता है; सब प्रकार के यज्ञ परम् की प्राप्ति की ओर मार्ग हैं। इन विविध साधनों में एक आवश्यक चीज, जिसके होने से ही ये सब साधन बनते हैं, यह है कि निम्न प्रकृति को क्रियाओं को अधीनस्थ करना, कामना के प्रभुत्व को क्षीण करना और उसके स्थान पर किसी श्रेष्ठतर शक्ति को प्रतिष्ठित करना, उस दिव्यतर आनन्द के लिए निरे अहंकारमय भोग को त्याग देना जो कि यज्ञ से, आत्मोत्सर्ग से, आत्म-प्रभुत्व से, अपने निम्न आवेगों को किसी महत्तर और उच्चतर ध्येय पर न्यौछावर करने से प्राप्त होता है।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।। ३१।।
३१. जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का उपभोग करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ नहीं करता उसके लिये यह लोक भी नहीं है तब फिर कोई दूसरा कैसे हो सकता है?
यज्ञ ही विश्व का विधान है, यज्ञ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, न इस लोक में प्रभुत्व प्राप्त हो सकता है, और न इस लोक के परे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, और न ही परमपद की उपलब्धि हो सकती है....
"यज्ञ से बचे हुए अमृत के उपभोग" का अर्थ है कि जब हम यज्ञ करते हैं, किसी हेतु के लिए अपनी ऊर्जा देते हैं तो उससे आनन्द उत्पन्न होता है। क्रिया करने में जो शारीरिक, प्राणिक और मानसिक ऊर्जा व्यय होती है उसका जो प्रतिफल हमें मिलता है, उसमें व्यय की गई ऊर्जा के अतिरिक्त जो भाग शेष बचता है, वह हमारे पुराणों के अनुसार भगवान् शंकर का भाग होता है। अर्थात् हमारी व्यय की हुई ऊर्जा के अतिरिक्त जो ऊर्जा शेष रह जाती है वह हमें भगवान् शिव को, जो कि परमात्मा के परात्पर स्वरूप हैं, उन्हें समर्पित करनी होती है। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे हमें हमारी आत्मा के उत्थान में परात्पर देव भगवान् शंकर को, या फिर श्रीमाताजी को अर्पण करना होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। यदि हमने उसका उपयोग अपनी इन्द्रियों आदि के तुष्टिकरण में किया तो वह भाग राक्षसों आदि को अर्पित हो जाता है और फिर आरोहण नहीं हो सकता।
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।। ३२॥
३२. इस प्रकार ये सब और दूसरे बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख में (अर्थात् उस ब्रह्मरूप अग्नि के मुख में जो समस्त हवियों को ग्रहण करता है) विस्तृत हुए हैं; उन सबको तू कर्म से उत्पन्न हुए जान; इस प्रकार जान लेने पर तू मुक्त हो जाएगा।
.....ये सब कर्म में प्रतिष्ठित उसी एक महान् सत् (Existence) के साधन और रूप हैं, जिन साधनों के द्वारा मानव-जीव का कर्म उसी 'तत्' (That) को समर्पित हो सकता है जिसका कि उसका बाह्य जीवन एक अंश है और जिसके साथ कि उसकी अंतरतम सत्ता एक है। ये सब 'कर्म से उत्पन्न होते हैं: सब भगवान् की उसी एक विशाल शक्ति से निकलते और उसी के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं जो विश्वकर्म में अपने-आप को अभिव्यक्त करती और इस विश्व के समस्त कर्म को उसी एक परमात्मा और परमप्रभु का उत्तरोत्तर वर्धनशील नैवेद्य या भेंट बनाती है जिसकी अंतिम अवस्था मानव-प्राणी के लिए आत्म-ज्ञान की या भागवत् चेतना की या ब्राह्मी चेतना की प्राप्ति है। 'ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा - एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।'
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।। ३३ ।।
३३. हे परंतप ! द्रव्य आदि से अनुष्ठित होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ होता है; हे पार्थ ! सभी कर्म ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं (किसी निम्नतर ज्ञान में नहीं अपितु उच्चतम आत्मज्ञान तथा ईश्वरज्ञान में)।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।। ३४।।
३४. उस ज्ञान को तू गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, विविध प्रकार से प्रश्न करते हुए और गुरु की सेवा के द्वारा सीख; ऐसे ज्ञानी मनुष्य जिन्होंने वस्तुओं के सच्चे स्वरूप का दर्शन किया है (न कि वे जो केवल बुद्धि से जानते हैं) तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे।
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ।। ३५।।
३५. हे पाण्डव ! जिस ज्ञान को प्राप्त कर के फिर तू इस मोह में नहीं फंसेगा; क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष रूप से आत्मा में और फिर मुझ में देखेगा।
जिसमें सब कुछ की परिसमाप्ति होती है वही वह ज्ञान है जिसके द्वारा 'तू सब भूतों को निःशेष रूप से आत्मा के अन्दर और फिर मेरे अन्दर देखेगा।' क्योंकि आत्मा वही एक अखण्ड, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी, स्वयं-सत् यथार्थता या ब्रह्म है जो हमारे मनोमय पुरुष के पीछे छिपा हुआ है जिसमें हमारी चेतना अहंभाव से मुक्त होने पर विशालता को प्राप्त होती है और तब हम सभी जीवों को उसी एक स्वयं-सत् के अन्दर 'भूतानि' के रूप में देख पाते हैं।
परन्तु हम देखते हैं कि यह आत्मतत्त्व या अक्षर ब्रह्म हमारी मूलभूत मनोवैज्ञानिक चेतना के प्रति उन परम् पुरुष का आत्म-निरूपण है जो हमारी सत्ता के स्रोत हैं और जो कुछ क्षर या अक्षर है वह सब उन्हीं की अभिव्यक्ति है। वे ही ईश्वर, भगवान्, पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं को हम सभी कुछ यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं; उन्हीं के हाथों में हम अपने सब कर्म सौंप देते हैं; उन्हीं की सत्ता में हम जीते और गति करते हैं; हमारी प्रकृति में उनके साथ एकीभूत होकर और उन्हीं में सब जीवों के साथ एक होकर, हम उनके साथ और जीवमात्र के साथ एक-जीव, सत्ता की एक-शक्ति हो जाते हैं; उनकी परम् सत्ता के साथ हम अपनी आत्म-सत्ता को तद्रूप और एक कर लेते हैं। काम का वर्जन कर यज्ञ के लिए कर्मों के करने से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और आत्मा की स्वयं की उपलब्धि तक पहुँचते हैं; आत्मज्ञान और परमात्मज्ञान में स्थित होकर कर्म करने से हम भागवत् सत्ता की एकता, शान्ति और आनन्द में मुक्त हो जाते हैं।
गीता एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से कहती है कि द्रव्य आदि से अनुष्ठित होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ होता है। ज्ञान-यज्ञ से क्या तात्पर्य है? एक विकल्प तो यह है कि हम ज्ञान को सुख-साधन आदि जुटाने के लिये, मन, प्राण, शरीर की अनेकों प्रकार की तुष्टियों की पूर्तियों के लिये अपने अहं की ओर मोड़ सकते हैं, अथवा दूसरा विकल्प है कि हम उसे परमात्मा की सेवा में लगा दें। हम अपनी सारी क्षमताओं को श्रीमाताजी की सेवा के लिये अर्पित कर दें। यही सच्चा ज्ञान-यज्ञ है।
दूसरी बात यहाँ गीता बता रही है कि सभी कर्म ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं (किसी निम्नतर ज्ञान में नहीं अपितु उच्चतम आत्मज्ञान तथा ईश्वरज्ञान में)। यज्ञ रूप से किये जायें तभी कर्मों की समाप्ति ज्ञान में होती है अन्यथा तो वे केवल एक बाहरी क्रिया मात्र होते हैं। जैसे-जैसे कर्म उन्नत होंगे वैसे-वैसे ज्ञान अधिक समुन्नत होगा और जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे-वैसे कर्म और अधिक उन्नत होंगे। परंतु हम यज्ञ रूप कर्म शुरू कैसे करें? व्यक्ति अपनी समझ और शक्ति-सामर्थ्य के भरोसे कर्मयज्ञ करने लगे, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए यदि व्यक्ति को सम्यक् ज्ञान चाहिये तो उसे गुरु की शरण में जाना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना होगा जिसे इस चीज का भली-भाँति ज्ञान है। उनसे सीखकर हम यह यज्ञ आरंभ कर सकते हैं। और जब ऐसा यज्ञ संपन्न हो जाएगा तब व्यक्ति सभी भूतों को पूर्ण रूप से आत्मा में और फिर 'मुझमें' अर्थात् पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण में देखेगा।
यहाँ यज्ञ का प्रसंग अर्जुन के इस प्रश्न से उठा कि निष्काम कर्म कैसे करें? क्योंकि हमेशा ही कर्मों के हेतु के रूप में कामना तो रहती ही है। फिर कौनसा कर्म करना चाहिये और कौनसा नहीं करना चाहिये, इसका पता भी नहीं लगा पाते। इसलिये यहाँ गीता बताती है कि हमें कर्म यज्ञ-रूप में और पुरुषोत्तम के निमित्त करने चाहिये। शुरू में हमारी समझ स्थूल होगी, बड़ी सीमित होगी। परंतु जैसे-जैसे हम परमात्मा के निमित्त कर्म करने प्रारम्भ करेंगे वैसे-वैसे उनकी शुद्धि होनी प्रारम्भ हो जायेगी। फिर जैसी हमारी संरचना होगी वैसे-वैसे हम हमारे सभी कर्म परमात्मा के निमित्त करना प्रारम्भ कर देंगे। धीरे-धीरे हम अपनी दैनंदिन भौतिक क्रियाकलापों को, उसके बाद उससे कुछ गहरी चीजों को अधिकाधिक यज्ञ के रूप में करना शुरू कर देंगे।
और सभी कर्मों की समाप्ति ज्ञान में होती है इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान होने पर कर्म समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग इसका इसी रूप में अर्थ लगाते हैं कि ज्ञान होने के बाद कर्म समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा ही होता तो भगवान् अपनी सारी शिक्षा के बाद अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त ही कैसे कर सकते थे? इसका अर्थ यह है कि ज्ञान होने पर हमारे कर्म और अधिक परिशुद्ध हो जाते हैं और वे हमें अधिक उच्चतर ज्ञान में ले जाते हैं। और उस उच्चतर ज्ञान से हमारे कर्म और अधिक दिव्य बन जाते हैं। इस प्रकार कर्म और ज्ञान एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं और यज्ञ का आरोहण चलता रहता है।
IV. ज्ञान एवं कर्मयोग
गीता की शिक्षा के इस पहले भाग में योग और ज्ञान वे दो पंख हैं जिनसे जीव आरोहण करता है। योग से अभिप्रेत है निष्काम होकर, समस्त पदाथों और मनुष्यों के प्रति आत्म-समत्व रखकर, पुरुषोत्तम अथवा परम् पुरुष के लिए यज्ञरूप से किये गये दिव्य कर्मों के द्वारा भगवान् से एकता, जबकि ज्ञान वह है जिस पर यह निष्कामता, यह समता, यह यज्ञ-शक्ति प्रतिष्ठित होते हैं। दोनों पंख निश्चय ही उड़ान में एक-दूसरे की सहायता करते हैं; दोनों एक साथ क्रिया करते रहते हैं, फिर भी इस क्रिया में बारी-बारी से एक-दूसरे की सहायता करने का सूक्ष्म क्रम रहता है, जैसे मनुष्य की दोनों आँखें बारी-बारी से देखती हैं इसीलिए एक साथ देख पाती हैं, इसी प्रकार योग और ज्ञान अपने सारत्तत्त्व के परस्पर आदान-प्रदान के द्वारा एक-दूसरे को संवर्द्धित करते रहते हैं। ज्यों-ज्यों कर्म अधिकाधिक निष्काम, समचित्त और यज्ञभावापन्न होते जाते हैं, त्यों-त्यों ज्ञान वर्धित होता है; ज्ञान के वर्धन के साथ ही जीव अपने कर्म की निष्काम और यज्ञात्मक समता में अधिकाधिक दृढ़ होता जाता है। इसलिए गीता ने कहा कि किसी द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है।
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ।। ३६ ।।
३६. यदि तू समस्त पापियों से भी अतिशय पाप करनेवाला है तब भी, उस समस्त पाप की कुटिलता-रूप समुद्र को ज्ञान-रूप नौका के द्वारा निश्चय ही पार कर जाएगा।
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुते ऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।। ३७।।
३७. हे अर्जुन ! जैसे प्रज्ज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मीभूत कर देती है वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्मीभूत कर देती है।
इसका कदापि यह अभिप्राय नहीं है कि जब ज्ञान पूर्ण होता है तब कर्म का विराम हो जाता है। इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है इसे गीता द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है जब वह ऐसा कहती है कि 'योगसंन्यस्तकर्माणं आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति' अर्थात् जिसने ज्ञान के द्वारा अपने सब संशयों को काट डाला है और योग के द्वारा कर्मों का संन्यास किया है वह आत्मवान् पुरुष अपने कर्मों से नहीं बँधता, और फिर गीता का यह वचन कि, कुर्वन्नपि न लिप्यते अर्थात् जिसकी आत्मा सब भूतों की आत्मा हो गयी है वह कर्म करता हुआ भी अपने कर्मों में लिप्सत नहीं होता, उनमें फँसता नहीं, वह उनसे आत्मा को बंधन में डालनेवाली कोई प्रतिक्रिया ग्रहण नहीं करता।
गीता कह रही है कि यदि हम में बहुत विकृतियाँ हैं, हमारे कमों में संतुलन नहीं है और वे सभी अहं के नाना प्रकार के आवरणों से, राग-द्वेष, लोभ, मोह, या अन्य किन्हीं निम्न तुष्टियों से चालित हैं तो इस सब असंतुलन का परिणाम तो हमें भुगतना ही होगा। ये ही हमारे पापों के परिणाम हैं। और जब हमें ज्ञान होता है तब हमारी सभी निम्न गतियाँ खत्म हो जाती हैं और हम एक उच्चतर समन्वय में निवास करना प्रारम्भ कर देते हैं और उस सन्तुलन में होने के कारण उसके कोई दुष्परिणाम नहीं होते। इसे इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।
दूसरी बात है कि 'जैसे प्रज्ज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मीभूत कर देती है वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्मीभूत कर देती है।' गीता का कर्मों से तात्पर्य बड़ा विचित्र है। 'जो कर्मों में भी अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्मों को देखता है वही सच्चा विवेकी है, वही अहं-शून्य है।' अर्थात् जब हम किसी हेतु या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और निम्न चेतना के द्वारा कोई प्रयास या चेष्टा करते हैं और अपने-आप को उसका कर्ता मानते हैं, तब वह कर्म होता है। और दूसरी ओर यदि हम यह देखते हैं कि कर्म तो परमात्मा की परा प्रकृति कर रही है, हम तो उसके हाथों में यंत्र-मात्र हैं या फिर हम केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिये पराप्रकृति की क्रिया में सहमति दे रहे हैं और उसमें सहभागी हो रहे हैं तब फिर वे कर्म हमारे अपने नहीं रह जाते। गीता में भगवान् ने अर्जुन को स्पष्ट कहा है कि 'यदि तू तेरे अहं के वशीभूत होकर और यह सोचकर युद्ध करेगा कि कौरव पापी हैं और उन्होंने तेरे साथ अन्याय किया है इसलिये उन्हें दण्ड मिलना चाहिये, तो तू पाप का भागी होगा। वहीं यदि तू मेरी आज्ञा मान कर युद्ध करेगा तो तुझे सम्पूर्ण त्रिलोकी को नष्ट करने पर भी कोई पाप नहीं लगेगा।' क्योंकि ऐसा करने में वह भगवान् के आदेश का ही पालन कर रहा होगा। अतः जब व्यक्ति को यह सच्चा ज्ञान हो जाता है कि परम् प्रभु की शक्ति ही है जो उनकी प्रसन्नता के लिये सारे कर्म करती है, और इस प्रकार देखते हुए जो अपनी इन्द्रियों को उसी के अनुसार क्रिया में प्रवृत्त करता है, वह फिर कर्म करते हुए भी अकर्ता होता है। गीता के अकर्ता के सिद्धांत से तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति सब काम छोड़ कर निष्क्रिय बैठ जाये। यदि व्यक्ति कर्म छोड़कर निष्क्रिय बैठता है तो इसका अर्थ है कि वह दुराग्रह से ग्रसित है और तामसिक है। क्योंकि वह कर्मों को अपने भौतिक, प्राणिक और मानसिक आवेगों और उनसे होने वाली अहं की तुष्टियों को प्राप्त करने या फिर उनमें आने वाले संकटों को टालने के लिये करता है। यही तामसिक यज्ञ, तप, दान, और श्रद्धा आदि के संबंध में भी है। इसलिये सच्चा कर्म तो वह है जो भगवान् की दिव्य प्रकृति करती है, बाकी सब अकर्म है। यह सब चर्चा आगे चलकर त्याग और संन्यास के विषय में भी आएगी। त्याग कर्मों का नहीं करना होता, अपितु उन कमाँ के पीछे को उन कामनाओं और वासनाओं का करना होता है जो उन कमाँ को दूषित करती हैं। वास्तव में, कर्मों के त्याग का कोई औचित्य भी नहीं है और ऐसा करना संभव भी नहीं है। उदाहरण के लिए, जब हम देखें कि हमारे सभी सम्बन्ध मोह से ग्रसित हैं और स्व पर केन्द्रित हैं, तो एक मनोभाव तो यह हो सकता है कि इस विकृति से बचने के लिए हम सभी संबंधों को ही काट डालें और शुष्क हो जाएँ। ऐसा करने में परमात्मा की ओर ले जाने वाली सबसे शक्तिशाली शक्ति, 'प्रेम', से हम वंचित रह जाएँगे, और निपट शुष्क संन्यासी बन जायेंगे और ऐसे में जीवन में कोई मृदुलता, कोई हँसी, कोई भाव नहीं रह जाएगा और हम एक नकारात्मकता और कठोर दुराग्रह से ग्रसित एक स्वार्थमय जीव बनकर रह जाएँगे। दूसरा है एक सकारात्मक दृष्टिकोण जिसके अनुसार हमें प्रेम करने से नहीं रुकना चाहिये अपितु जो तत्त्व उसे दूषित करता है, उसका निवारण करना चाहिये और सही रूप से प्रेम करना चाहिये। यदि हमारे सम्बन्ध गलत आधार पर हैं, अपनी अहं की तुष्टि के आधार पर ही हैं, तो उन्हें सही आधार पर स्थापित करना होगा, न कि सभी संबंधों को ही खत्म कर देना होगा। जब सम्पूर्ण सृष्टि और उसमें सभी जीव आपस में अविभाज्य रूप से एक हैं तो हम स्वयं को अलग कर ही कैसे सकते हैं। यह संभव ही नहीं है। उसके लिए प्रयत्न करना तो मूर्खता है और स्वयं अपनी अखंडता और भगवत्ता का ही खंडन करना है।
परंतु हमारी बाहरी प्रकृति का जैसा गठन है, वह निम्न चीजों में और विकारों में गिरने की ओर ही वृत्ति रखती है। और इसीलिए संन्यास और निवृत्तिपरक वृत्ति पर बल दिया जाता है। परंतु ऐसा करना तो अपेक्षाकृत रूप से आसान है कि व्यक्ति अपने-आप को संबंधों से अलग कर ले और ऐसी व्यवस्था कर ले कि अहं को, स्वार्थ को कोई मौका ही न मिले, पर यह कोई सच्चा उपाय नहीं है। जबकि यह भी सत्य है कि संबंधों के होते हुए उनके विकारों को दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा एक क्षण में ही हो जाए, यह संभव नहीं है। हमें धैर्य रखना होगा। इसको शुरू करने के लिये यह संकल्प करना होगा कि हम अपने-आप को, जैसे हम हैं वैसे के वैसे को ही श्रीमाताजी को सौंप दें और इसे अपने ही संसाधनों के आधार पर ठीक करने की कोशिश न करें। क्योंकि जैसे ही हम इसे ठीक करने का दृष्टिकोण अपनाते हैं तुरन्त ही अहं एक नया भेष बना कर घुस आता है कि, 'मैं इसे ठीक करूँगा', 'मैं श्रीमाताजी की सेवा करूंगा, उनका प्रयोजन सिद्ध करूँगा' अथवा 'मेरी साधना हो जायेगी' आदि-आदि। अतः हमें सच्चे रूप से इसका संकल्प कर के अपने गुणों-अवगुणों, अपनी कमियों, अपने सभी कुछ की गठरी बाँध कर श्रीमाताजी के हाथों में सौंप देनी होगी। तब फिर वे हमसे चाहे जैसा कर्म करा लें, उसके लिये हम तैयार हों। हालाँकि व्यवहार में ऐसा हो पाना इतना आसान नहीं है और इस भाव को प्राप्त करने में समय लगता है। इस प्रक्रिया में हमारे निम्न भाग हमें धोखा देंगे, अपने उत्पात करेंगे, परन्तु श्रीमाँ हमारा मार्गदर्शन करेंगी। तब फिर वे हमें और हमारे अहं को जितना चाहें अपने काम में लें। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप न होगा। यदि हम अपनी अहमात्मक चेतना से ही अहं का निषेध करने का और उससे मुक्त होने का प्रयास करें तो यह कैसे संभव हो सकता है। यदि उसे श्रीमाँ को समर्पित कर दिया जाए तब फिर वे उसे अपनी इच्छानुसार काम में लें। तभी हम सच्चे रूप से संबंध बना सकेंगे और उनमें कोई विकार और कोई बंधन नहीं रह जाएगा। जो भी चीज हम अपने-आप के लिए बचा रखने का, अपने अहं की तुष्टि के रूप में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, वही हमारे पथ में बाधक बन जाती है। सभी कुछ को उन्हीं के हाथों में छोड़ देना होगा, और तब फिर वे स्वयं जैसा, जब, जहाँ और जो करवाना चाहें वैसा स्वयं ही करवा लेंगी और इसमें कोई विकार भी न होगा। तब सभी चीजें भगवान् के काम आने लग जाती हैं। यह सच्चा समाधान है। गीता भी यही कहती है।
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।। ३८ ।।
३८. इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र निश्चय ही कुछ भी नहीं है; योग के द्वारा सिद्ध हुआ पुरुष उस ज्ञान को उपयुक्त समय आने पर अपने-आप अपने भीतर प्राप्त करता है।
यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है इसका वर्णन करते हुए गीता कहती है कि पहले इस ज्ञान की उन तत्त्वदर्शी ज्ञानियों से दीक्षा लेनी होती है, जो केवल बुद्धि से ही नहीं जानते हैं अपितु जिन्होंने इसके सारभूत सत्यों को प्रत्यक्ष देखा है; परन्तु वास्तविक ज्ञान तो हमें अपने अन्दर से ही मिलता है : 'योग के द्वारा सिद्ध हुआ पुरुष उस ज्ञान को उपयुक्त समय आने पर अपने-आप अपने भीतर प्राप्त करता है', अर्थात् यह ज्ञान उस मनुष्य में संवर्द्धित होता रहता है और ज्यों-ज्यों वह मनुष्य निष्कामता, समता और भगवद्भक्ति में बढ़ता जाता है त्यों-त्यों ज्ञान में भी बढ़ता जाता है। परन्तु यह बात केवल परम् ज्ञान के सम्बन्ध में ही पूर्ण रूप से कही जा सकती है, क्योंकि जो ज्ञान मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा एकत्रित करता है उसे तो वह इन्द्रियों और तर्कशक्ति के द्वारा परिश्रम कर के बाहर से ही इकट्ठा करता है।
'ज्ञान' शब्द भारतीय दर्शनशास्त्रों और योगशास्त्रों में सर्वत्र इसी परम् आत्म-ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है; यह वह ज्योति है जिसके द्वारा हम अपनी सत्य-सत्ता में संवर्द्धित होते हैं, न कि कोई ऐसा ज्ञान है जिससे हम अपनी जानकारी और अपनी बौद्धिक संपत्तियों को वर्धित करते हैं; यह कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक या नैतिक या सौंदर्यात्मक अथवा लौकिक और व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। ये सब भी निस्संदेह हमें उन्नति में सहायता करते हैं पर ये हमारी संभूति (अभिव्यक्ति) के विकास में सहायक होते हैं, हमारी आंतरिक सत्ता के विकास में नहीं। यौगिक ज्ञान की परिभाषा में इनका समावेश तब होता है जब हम इनसे परमात्मा, आत्मा, भगवान् को जानने में सहायता लें। भौतिक विज्ञान को हम यौगिक ज्ञान तब बना सकते हैं जब हम उसकी प्रक्रियाओं और बाह्य घटनाओं के आवरण को भेद कर उस एकमात्र सद्वस्तु को देख लें जो सभी कुछ को स्पष्ट कर देती है; मनोवैज्ञानिक विद्या को यौगिक ज्ञान तब बनाया जा सकता है जब हम उससे अपने-आपको जान सकें और निम्नतर और उच्चतर का विवेक कर सकें जिससे कि निम्न अवस्था को त्याग कर हम उच्च अवस्था में संवर्द्धित हो सकें; दर्शन-संबंधी ज्ञान को हम यौगिक ज्ञान तब बना सकते हैं जब हम इसे अस्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर एक प्रकाश के रूप में ढाल सकें जिससे कि उसे खोज सकें और उसमें निवास कर सकें जो शाश्वत है। नैतिक ज्ञान को यौगिक ज्ञान तब बनाया जा सकता है जब इससे पाप और पुण्य के भेद को जान कर हम, पाप को दूर करें और पुण्य से ऊपर उठकर दिव्य प्रकृति की पूर्ण निर्मलता में पहुँच जाएँ, सौंदर्यात्मक बोध को हम यौगिक ज्ञान तब बना सकते हैं जब हम इसके द्वारा भगवान् के सौंदर्य को खोज लें, लौकिक ज्ञान को हम यौगिक तब बना सकते हैं जब हम उसके भीतर से ईश्वर के अपनी सृष्टि के साथ व्यवहार को देख पाएँ और फिर उस ज्ञान का उपयोग मनुष्य में रहनेवाले भगवान् की सेवा के लिए करें। परंतु तब भी ये विद्याएँ सच्चे ज्ञान की सहायक भर होती हैं; वास्तविक ज्ञान तो वही है जो मन के लिए अगोचर है, मन जिसका केवल आभासमात्र प्राप्त करता है, जो आत्मा में रहता है।
आम शिक्षा-प्रणाली में विद्यार्थी को जो भी जानकारियाँ या हुनर सिखाएँ जाते हैं उनसे वास्तव में शिक्षा नहीं होती। ऐसी शिक्षा से व्यक्ति के आंतरिक गठन में तो वास्तव में कोई सुधार नहीं आता। इतना भर कहा जा सकता है कि इस प्रशिक्षण से व्यक्ति जो पहले कर रहा था उसी को अधिक सुचारू ढंग से कर पाएगा, परंतु उसकी गुणवत्ता में तो वास्तव में कोई बदलाव आएगा नहीं। और यदि आंतरिक गठन ही दोषपूर्ण हो तो गुणवत्ता में लाभ की बजाय गिरावट ही आ जाएगी। क्योंकि उससे कोई आत्मिक विकास तो होगा नहीं और विद्यार्थी अपने गठन के अनुसार उसका उपयोग या दुरूपयोग अधिक दक्षता से करेगा। अतः शिक्षा से तात्पर्य है आत्मा का संवर्धन और उसकी मन, प्राण और शरीर में अभिव्यक्ति। यही शिक्षा है। यहाँ दिव्य गुरु कह रहे हैं: इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र निश्चय ही कुछ भी नहीं है; योग के द्वारा सिद्ध हुआ पुरुष उस ज्ञान को उपयुक्त समय आने पर अपने-आप अपने भीतर प्राप्त करता है।
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।। ३९।।
३९. जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त है, जिसने अपने मन और इन्द्रियों को अपने वश में कर लिया है, जिसने अपनी सम्पूर्ण चेतन सत्ता को उस परम् पुरुष में स्थिर कर दिया है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर के अविलम्ब परा शान्तिर को प्राप्त कर लेता है।
वास्तव में जीवन में सारी क्रिया ही केवल श्रद्धा की है और किसी चीज की नहीं। श्रद्धा के अंदर स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है। यदि श्रद्धा है तो वह अभिव्यक्त होकर रहेगी। यह अलग बात है कि अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में मन, प्राण, शरीर की अपनी-अपनी कमियाँ, अपना-अपना गठन रहता है जिनकी अपनी-अपनी क्रियाएँ चलती रहती हैं। इसलिये आवश्यक नहीं है कि ये भाग प्रारम्भ से ही श्रद्धा के अनुरूप सहयोगी हों। परन्तु चाहे ये सब साथ आयें या नहीं, काम तो वही होगा जिसमें हमारी वास्तविक श्रद्धा है। शुरू में हम भ्रमित हो सकते हैं परन्तु चाहे किन्हीं भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरीकों से हो, आखिरकार श्रद्धा ही हमें प्रेरित करेगी और हमारे सभी भागों का एक निश्चित दिशा में संचालन करेगी। हमारा वर्तमान जीवन पूर्व की श्रद्धा का परिणाम है और वर्तमान श्रद्धा हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे भीतर भागवत् संकल्प का क्या औचित्य होता। भागवत् संकल्प की अभिव्यक्ति में अनेक सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जाएँ अपना-अपना काम करती रहती हैं। परंतु वास्तव में तो इन सबका अंतिम परिणाम अंतरतम श्रद्धा की अभिव्यक्ति ही है। श्रद्धा के पीछे जो सत्य है वह इतना बहु-आयामी है कि हमारे मन, प्राण और शरीर उसका गठन नहीं कर सकते। और इस प्रक्रिया में हमारे समस्त विद्रोह, अविश्वास आदि भी अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं और अंततः परिणाम श्रद्धा के अनुरूप ही होता है। हमारा मन भले कितना भी विकसित और समृद्ध क्यों न हो, परंतु फिर भी वह श्रद्धा को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। व्यक्ति जो भी कार्य प्रारम्भ करता है वह श्रद्धा की शक्ति से ही करता है फिर वह चाहे योग हो या अन्य कोई कार्य। कार्य की संसिद्धि होने तक श्रद्धा व्यक्ति को बार-बार उसी दिशा में प्रवृत्त करती रहती है। यह जीवन का मूलभूत सत्य है। यदि ऐसा न होता तो हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते थे।
यदि हमारी समझ और सोच ही सब कुछ होते तब तो श्रीअरविन्द और श्रीमाँ का योग संभव ही न होता क्योंकि अतिमानसिक रूपान्तरण तो धरती पर आज तक कभी संसिद्ध हुआ नहीं। इसलिये श्रद्धा के सिवा इस योग का और कोई आधार ही नहीं है। यह केवल श्रद्धा से ही संभव है और वही हमें इस महत् प्रयास में लगाये रखती है। श्रद्धा वह डोर है जो परमात्मा हमारे लिए नीचे डालते हैं जिसे पकड़ कर हम ऊपर आरोहण कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम निम्न प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा सकते हैं। 'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं'। यह जीवन की केन्द्रीय चीज है। इसके अलावा जीवन में कुछ और है ही नहीं। जो हमारी श्रद्धा है वह अवश्य ही चरितार्थ की जा सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है।
अज्ञश्वाश्रद्दधानश्व संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ।। ४०।।
४०. जो अज्ञ है और श्रद्धा से रहित है और संशय से युक्त है वह नष्ट हो जाता है; संशय करनेवाले मनुष्य के लिये न यह लोक है न ऊपर का लोक है और न कोई सुख ही है।
वस्तुतः, यह सच है कि बिना श्रद्धा के न ही इस जगत् में कोई निर्णायक चीज प्राप्त हो सकती और न ही परलोक की कोई भी निधि प्राप्त की जा सकती; और केवल किसी सुनिश्चित आधार और वास्तविक सहारे को पकड़ने पर ही व्यक्ति किसी परिमाण में लौकिक या पारलौकिक सफलता, संतोष और सुख को प्राप्त कर सकता है; महज संशयशील मन अपने-आपको शून्य में खो देता है। परन्तु फिर भी निम्नतर ज्ञान में संदेह और अविश्वास होने के तात्कालिक उपयोग हैं; किन्तु उच्चतर ज्ञान में ये मार्ग के रोड़े हैं: क्योंकि वहाँ सारा रहस्य निम्नतर भूमिका की तरह सत्य और भ्रान्ति का सन्तुलन करना नहीं अपितु स्वतःप्रकाशमान सत्य की सतत्-प्रगतिशील अनुभूति करना है। बौद्धिक ज्ञान में सदा ही असत्य अथवा अपूर्णत्व का मिश्रण रहता है जिसे हटाने के लिये स्वयं सत्य को संशयात्मक परीक्षण की कसौटी से गुजारना पड़ता है; परन्तु उच्चतर ज्ञान में असत्य नहीं घुस सकता और इस या उस मत पर आग्रह कर के बुद्धि जो भ्रम ले आती है वह केवल तर्क के द्वारा दूर नहीं होता, अपितु वह तो अनुभूति में सुदृढ़ रूप से लगे रहने से अपने-आप ही दूर हो जाता है।
------------------------------------------------
"आध्यात्मिक अर्थ में श्रद्धा कोई मानसिक विश्वास नहीं है जो विचलित हो सके और बदल सके। मन में यह ऐसा रूप ले सकती है, पर वह विश्वास स्वयं श्रद्धा नहीं है, वह तो उसका केवल बाहरी रूप है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर, बाहरी आकृति तो बदल सकतो है पर आत्मा वही बनी रहती है, वैसी ही बात यहाँ भी है। श्रद्धा अन्तरात्मा में विद्यमान एक निश्चयता है जो तर्क-बुद्धि पर, किसी एक या दूसरे मानसिक विचार पर, परिस्थितियों पर, मन या प्राण या शरीर को किसी एक या दूसरी क्षणिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती श्रद्धा अनुभव पर निर्भर नहीं करती; यह कोई ऐसी चीज है जो अनुभव के पूर्व से हो रहती है। जब व्यक्ति योग प्रारंभ करता है, तो ऐसा वह प्रायः अनुभव की शक्ति पर नहीं अपितु श्रद्धा को शक्ति पर करता है। ऐसा केवल योग और आध्यात्मिक जीवन के विषय में ही नहीं अपितु सामान्य जीवन के बारे में भी है। सभी कर्मप्रधान लोग, खोजकर्ता, आविष्कारक, ज्ञान के प्रकाशक श्रद्धा से ही आरंभ करते हैं और जब तक प्रमाण नहीं मिल जाता या कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे निराशा, असफलता, प्रमाणों के अभाव व अस्वीकृति के उपरान्त भी प्रयास जारी रखते हैं, और ऐसा वे अपने अंदर किसी ऐसी चीज के कारण करते हैं जो उनसे कहती है कि यही सत्य है, यही वह चीज है जिसका अनुसरण करना होगा और जिसे सिद्ध करना होगा... श्रद्धा अंतरात्मा का किसी ऐसी चीज के विषय में साक्ष्य है जो अभी तक अभिव्यक्त, संसिद्ध या अनुभूत नहीं हुई है, परंतु फिर भी जिसे हमारे अंदर का 'ज्ञाता' सभी लक्षणों के अभाव में भी सत्य या अनन्य रूप से अनुसरण करने तथा प्राप्त करने योग्य अनुभव करता है। हमारे भीतर की यह चीज तब भी बनी रह सकती है जब मन में कोई दृढ़ विश्वास न हो, तब भी जब प्राण संघर्ष, विद्रोह और इंकार करता हो। ऐसा कौन है जो योगाभ्यास करता हो और जिसके ऐसे दौर न आते हों, निराशा, असफलता, अविश्वास और अंधकार के लंबे दौर? परंतु कोई ऐसी चीज है जो उसे थामे रखती है और उसकी अपनी (सामर्थ्य-असामर्थ्य) के बावजूद भी बनी रहती है, क्योंकि उसे यह अनुभव होता है कि जिस चीज का उसने अनुसरण किया वह सही थी, तथा वह ऐसा अनुभव हो नहीं करता अपितु जानता है।
प्राप्त ज्ञान में जो कुछ भी अपूर्णता रह गयी हो उसे अवश्य दूर करना होगा, किन्तु यह काम जो अनुभूति हो चुकी है उसके मूल पर संदेह करने से नहीं अपितु आत्मा में अधिक गहरे, ऊँचे और अधिक विशाल जीवन जीने से और आगे की तथा पूर्णतर अनुभूति की ओर बढ़ने के द्वारा होगा। और जो कुछ अभी अनुभूत नहीं हुआ है उसके लिये श्रद्धा के द्वारा तैयारी करनी होगी, न कि संशयपूर्ण पूछताछ से, क्योंकि यह ऐसा सत्य है जिसे बुद्धि नहीं दे सकती, और तार्किक तथा यौक्तिक मन जिन विचारों में उलझा रहता है यह वस्तुतः बहुधा उनसे सर्वथा विपरीत होता है। यह ऐसा सत्य नहीं है जिसे प्रमाणित करने की आवश्यकता हो, अपितु ऐसा सत्य है जिसे आंतरिक रूप से जीना होता है, यह वह महत्तर सद्वस्तु है जिसके स्वरूप में हमें संवर्द्धित होना है।
श्रद्धा और संशय के संबंध में यह बहुत ही सुंदर व्याख्या है। श्रीअरविन्द कह रहे हैं कि जो श्रद्धावान् नहीं है अर्थात् जो संशयवादी है वह बड़ी विषम और दयनीय स्थिति में है।
अब कुछ लोगों के भीतर यह प्रश्न उठता है कि फिर संशय का क्या औचित्य है और हमें किस पर संशय करना चाहिये और किस पर नहीं। कुछ का तो मानना है कि या तो सभी कुछ पर संदेह करना चाहिये या फिर सभी कुछ पर विश्वास करना चाहिये।
आखिर हमारे अंदर संदेह या संशय क्यों उठता है? इसका कारण यह है कि हमारे भीतर जो श्रद्धा है उसका प्रतिबिंब हमारी बुद्धि में पूरी तरह से नहीं आ सकता। अतः जब तक हम बुद्धि के क्षेत्र तक सीमित हैं तब तक संशय की उपयोगिता रहती है क्योंकि संशय हमें गलत मार्ग पर चलते रहने से रोकता है। इसलिये स्वयं श्रद्धा पर तो संशय नहीं किया जा सकता परंतु जब तक उसका निरूपण बुद्धि में होता है तब तक संशय की उपयोगिता है। हमारी आन्तरिक गहराई में जो श्रद्धा है उस पर संशय नहीं किया जा सकता क्योंकि वह तो सत्य है और यदि उस पर ही संशय करेंगे तो हमारा सत्य की ओर आरोहण रुक जायेगा। बुद्धि के क्षेत्र में हमारे अनुभव की अभिव्यक्ति की क्षमता सीमित होती है क्योंकि आन्तरिक अनुभव को मानसिक रूप से अभिव्यक्त करने की प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग-अलग होती है।
-----------------------------------------------------
एकमात्र सुनिश्चित और सर्वसमन्वयात्मक सत्य, जो विश्व का आधार ही है, वह यह है कि जीवन एक अजन्मा आत्मा तथा आत्मसत्ता की अभिव्यक्ति है, और जीवन के गुप्त रहस्य की कुंजी है इस आत्मा का अपनी रची हुई सत्ताओं से सच्चा सम्बन्ध। इस सब जीवन के पीछे अपनी असंख्य अभिव्यक्तियों (becomings) को देखती सनातन पुरुष को एक दृष्टि है; इसमें सब ओर तथा सर्वत्र ही एक अव्यक्त कालातीत सनातन पुरुष द्वारा कालगत अभिव्यक्ति का समावरण (envelopment) और अंतर्लयन (penetration) है। परन्तु यह ज्ञान योग के लिए महत्त्वहीन होगा यदि यह केवल एक ऐसा बौद्धिक तथा दार्शनिक विचारमात्र हो जिसमें न कोई जीवन हो और न जिसका कोई फल हो; जिज्ञासु के लिये एकमात्र मानसिक अनुभूति ही पर्याप्त नहीं हो सकती। क्योंकि योग जिसकी खोज करता है वह केवल विचार या केवल मन का सत्य नहीं है, अपितु एक जीवंत और प्रकाशकारी अध्यात्म-अनुभव का शक्तिशाली क्रियात्मक सत्य है। हमारे अंदर एक सच्ची अनंत उपस्थिति का सतत् अन्तर्वासी और सर्वव्यापी सान्निध्य, सुस्पष्ट बोध, घनिष्ठ अनुभव तथा समागम और ठोस बोध एवं संस्पर्श सदा-सर्वदा और सर्वत्र जागृत रहना चाहिये। वह उपस्थिति हमारे संग एक ऐसी जीवंत और सर्वव्यापक सद्वस्तु के रूप में रहनी चाहिये जिसमें हम और सभी पदार्थ अस्तित्वमान होते, गति करते और क्रिया करते हैं। और उसे हमें हर समय और हर जगह मूर्त, गोचर एवं सभी वस्तुओं के निवासी के रूप में अनुभव करना होगा। यह हमें सब पदार्थों की सच्ची आत्मा के रूप में गोचर होना चाहिए, सबके अविनाशी सारतत्त्व के रूप में स्पर्श-योग्य होना चाहिए, सबकी अन्तरतम आत्मा के रूप में घनिष्ठ रूप से मिलन योग्य होना चाहिए। यहाँ सभी सत्ताओं में इस आत्मा और आत्म-तत्त्व को मानसिक विचार द्वारा कल्पित करना ही नहीं, अपितु उसे देखना, अनुभव करना, संवेदन प्राप्त करना तथा हर प्रकार से इसका संस्पर्श प्राप्त करना और उतने ही सुस्पष्ट रूप से सभी सत्ताओं को इस आत्मा और आत्मतत्त्व में अनुभव करना ही वह आधारभूत अनुभव है जिसे अन्य सभी ज्ञान को समावृत करना होगा।
वस्तुओं की यह अनन्त और नित्य आत्मा सर्वव्यापक सद्वस्तु है, सर्वत्र विद्यमान एक ही सत्ता है; यह एकमेव एकीकारक उपस्थिति है और भिन्न प्राणियों में भिन्न-भिन्न नहीं है। इससे विश्व में प्रत्येक आत्मा या प्रत्येक दृश्य पदार्थ के भीतर उसको पूर्णता में साक्षात्कार किया जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि, इसकी अनन्तता आध्यात्मिक और आधारभूत है न कि एक निरी देश मर्यादित असीमता या एक काल मर्यादित अंतहीनता है। एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणु में या काल के एक क्षण में भी वह अनन्त वैसे ही असंदिग्ध रूप में अनुभव किया जा सकता है जैसे कि युगों के विस्तार या सौर पिण्डों की पारस्परिक दूरी की अतिविशाल बृहत्ता में किया जा सकता है। उसका ज्ञान या अनुभव कहीं भी शुरू हो सकता है और अपने आप को किसी भी वस्तु के द्वारा प्रकट कर सकता है; क्योंकि भगवान् सबमें हैं और सब कुछ भगवान् ही हैं।
अतः संशय की भूमिका केवल उस मानसिक अभिव्यक्ति तक ही है और श्रद्धा की जो प्रतिमूर्ति इस मानसिक चेतना में प्रकट होती है उसकी विकृतियों का परिमार्जन करना ही संशय का मूलभूत कार्य है। जो आन्तरिक अनुभव है वह तो सच्चा है उस पर संशय नहीं किया जाना चाहिये। यदि हमारे अनुभव में कोई कमी है अथवा कोई संकीर्णता है वह केवल अधिक गहरे अनुभव से ही दूर होगी। वह संशय से दूर नहीं हो सकती।
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।। ४१।।
४१. हे धनञ्जय अर्जुन ! जिस मनुष्य ने योग के द्वारा समस्त कमाँ का त्याग कर दिया है, ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों का विनाश कर दिया है, जो आत्मवान् है वह अपने कमाँ से नहीं बँधता है।
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।। ४२।।
४२. इसलिये हे भारत ! अज्ञान से उत्पन्न होनेवाले, हृदय में निवास करनेवाले अपने इस संशय को ज्ञानरूप तलवार के द्वारा काट कर योग का आश्रय ग्रहण कर (अनुष्ठान कर) और युद्ध के लिये खड़ा हो।
[आध्यात्मिक सत्य] अपने-आप में एक स्वयं-विद्यमान सत्य है और यह स्वयंसिद्ध भी होता यदि हम अज्ञान के इन्द्रजाल में वशीभूत हो न जी रहे होते। जो संदेह और व्यग्रताएँ हमें इस सत्य को स्वीकार करने और इसका अनुसरण करने से रोकती हैं, वे उसी अज्ञान से, इन्द्रियविमोहित और दुराग्रह-विमूढ़ मन और हृदय से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इनकी स्थिति निम्न और बाह्य सत्य में है और इसलिए उच्चतर सद्वस्तु के विषय में इन्हें संशय होता है, अज्ञानसंभूतं हृत्स्थं संशयं । गीता कहती है कि जिनके सत्य को जानने से सब कुछ जाना जाता है (यस्मिन् विज्ञाते सर्व विज्ञातम्) उन परमात्मा के साथ एकत्व में निवास कर, सतत् योगस्थ होकर, अनुभवगम्य ज्ञान के द्वारा, इस संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालना होगा।
इस प्रकार चौथा अध्याय 'ज्ञानयोग' समाप्त होता है।
पाँचवा अध्याय
I. ज्ञान, समता और कर्मयोग
[चौथे अध्याय के अन्तिम श्लोकों में श्रीकृष्ण ने यह घोषित किया। कि ज्ञान-यज्ञ ही सर्वोच्च है, समस्त कर्म ज्ञान में अपनी परिसमाप्ति पाते हैं, ज्ञान की अग्नि के द्वारा सब कर्म दग्ध हो जाते हैं; इसलिए वह व्यक्ति जो अपनी आत्मा को पा लेता है, वह योग के द्वारा कर्मों का त्याग व कर्मजनित बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्जुन पुनः विभ्रमित हो जाता है; क्योंकि निष्काम कर्म, जो कि योग का सिद्धांत है, और कर्म-संन्यास, जो कि सांख्य का सिद्धांत है, दोनों ही सिद्धांतों को इस प्रकार एक ही साथ रख दिया गया है मानो दोनों एक ही प्रक्रिया के भाग हों और फिर भी इनमें प्रत्यक्ष रूप से कोई तालमेल ही दिखाई नहीं देता। क्योंकि जिस तरह का समन्वय श्रीगुरु पहले ही दे चुके हैं - अर्थात् बाह्य अकर्म होने पर भी कर्म को होते हुए देखना और बाह्य कर्म में यथार्थ अकर्म को देखना, क्योंकि पुरुष अपने कर्त्तापन का भ्रम त्याग चुका है और अपने कर्म को यज्ञ के स्वामी के हाथों में सौंप चुका 3 - overline 95 अर्जुन की व्यावहारिक बुद्धि के लिये अत्यंत क्षीण, अत्यंत धुँधला और लगभग एक पहेलीनुमा भाषा में प्रकट किया गया है; उसने इसके आशय को नहीं समझा है या कम-से-कम इसके मर्म और इसकी वास्तविकता में प्रवेश नहीं कर सका है। इसलिए वह फिर पूछता है कि...
अर्जुन उवाच :
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्वितम् ।। १॥
१. अर्जुन ने कहा : हे कृष्ण ! आप मुझे कर्मों के संन्यास को बताते हो, और पुनः कर्मों के योग को कहते हो; इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उस एक को स्पष्ट सुनिश्चितता से मुझे बतलाइये।
भगवान् द्वारा दिया गया इसका उत्तर महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह योग और सांख्य के भेद को एकदम स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है और यद्यपि यह समन्वय की दिशा में विचार को पूर्णतः विकसित नहीं करता परंतु फिर भी उस समन्वय का संकेत अवश्य कर देता है।
श्रीभगवान् उवाच :
संन्यासः कर्मयोगश्व निःश्रेयसकरावुभौ ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।। २।।
२. श्रीभगवान् ने कहाः कर्मों का संन्यास और कमाँ का योग दोनों ही आत्मा को मोक्ष देने वाले हैं, किन्तु इन दोनों में कमाँ के संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ होता है।
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ।। ३।।
३. हे महाबाहो ! जो मनुष्य न द्वेष करता है और न कामना करता है उसे (कर्म करते हुए भी) नित्य संन्यासी जानना चाहिये; द्वन्द्वरहित होने के कारण वह बंधन से सरलता से और सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है।
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ।। ४।।
४. बालबुद्धि (अल्पबुद्धि) मनुष्य ही सांख्य और योग को एक-दूसरे से पृथक् बताते हैं, ज्ञानी ऐसा नहीं कहते; यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सम्यक् रूप से किसी भी एक के अनुष्ठान करने में प्रवृत्त करता है, तो वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है।
....क्योंकि अपनी संपूर्णता में ये दोनों ही एक-दूसरे को धारण किये हुए हैं।
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । ए
कं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।। ५।।
५. सांख्य मार्ग का अनुसरण करने वाले, ज्ञानयोगी संन्यासियों द्वारा जो पद प्राप्त किया जाता है वह योग मार्ग का अनुसरण करनेवाले योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है; जो मनुष्य सांख्य को और योग को एक ही देखता है वह यथार्थ देखता है।
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमासुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ।। ६।।
६. परन्तु हे महाबाहो! निष्काम योग के बिना संन्यास को प्राप्त करना कठिन है; जो मुनि योगयुक्त है वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
बाह्य संन्यास की कष्टकर प्रक्रिया (दुःखमाप्तुं) एक अनावश्यक प्रक्रिया है। यह पूर्णतः सत्य है कि सभी कर्मों को और साथ-ही-साथ कर्मफल को भी छोड़ना होता है, उनका त्याग करना होता है, परंतु आंतरिक रूप से, न कि बाह्य रूप से; ऐसा प्रकृति की जड़ता में नहीं किया जाता, अपितु उन अधीश्वर के प्रति यज्ञ रूप से किया जाता है, उस निर्व्यक्तिक ब्रह्म की शान्ति और आनन्द में किया जाता है जिसमें से बिना उसकी शान्ति को भंग किये सारा कर्म उत्पन्न होता है। कर्म का सच्चा संन्यास है समस्त कर्मों को ब्रह्म पर आश्रित करना...। इसीलिए गीता कहती है कि कर्मों के भौतिक संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि जहाँ संन्यास देहधारियों के लिए कठिन है, जिन्हें जब तक वे देह में हैं तब तक कर्म करना ही पड़ेगा, वहीं कर्मयोग अभीष्टसिद्धि के लिए सर्वथा पर्याप्त है और यह जीव को ब्रह्म के पास शीघ्रता और सरलता से ले आता है।
यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि गीता का आरम्भ कैसे हुआ तो हम पाएँगे कि शुरू में अर्जुन ने कहा कि उसे अपने परिजनों एवं गुरुजनों के रक्त से सना राज्य नहीं चाहिये। तब दिव्य गुरु उसे प्रचलित 'आर्य-क्षत्रिय धर्ममत' के अनुसार आत्मा के अमर होने और शरीर के नाशवान् होने आदि की बातें बताते हैं। क्योंकि अर्जुन को उसके वर्तमान स्तर से ही समझाना आरंभ किया जा सकता था, एकाएक ही अंतिम शब्द के लिए तो वह अभी तैयार नहीं था। हालाँकि उसके वर्तमान स्तर पर भी उसे किन्हीं भी बातों से सन्तोष नहीं हो सकता था क्योंकि उसके माध्यम से गीता को अपने गुह्यतम वचन तक पहुँचना है। सम्पूर्ण गीता उस चरम ज्ञान तक पहुँचने के लिए एक विकसित होता हुआ मार्ग है जिससे होकर व्यक्ति वहाँ तक पहुँच सके। जब अर्जुन 'आर्य-क्षत्रिय धर्ममत' से सहमत नहीं हुआ यद्यपि वह दिव्य गुरु के समक्ष शिष्य भाव से नतमस्तक हो उनसे प्रार्थना कर चुका था कि वे उसे ज्ञान दें कि उसे क्या करना चाहिये, तब भगवान् कहते हैं कि -
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।२.४०।।
इस मार्ग पर कोई भी प्रयास नष्ट नहीं होता, न ही कोई प्रत्यागमन ही होता है, इस धर्म का थोड़ा-सा अनुष्ठान भी महान् भय से मुक्त कर देता है।
आरम्भ में जब भगवान् ने निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया तो अर्जुन ने पूछा कि पहले तो बिना कामना के कर्म का चयन कैसे हो और फिर निष्काम कर्म संभव ही कैसे हो सकते हैं। तब दिव्य गुरु ने यज्ञ स्वरूप कर्म का उपदेश किया। इसके उपरान्त ज्ञान की बात आई कि सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में होती है और ज्ञानयोग ही सबसे पवित्र योग है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि जैसे ही व्यक्ति निष्काम कर्म की ओर चलेगा तो ज्ञान आएगा और जैसे ही ज्ञान में वृद्धि होती है तब व्यक्ति अधिक बेहतर तरीके से कर्म कर सकता है। इस प्रकार ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ज्ञानयोग और कर्मयोग एक पक्षी के दो पंखों के समान हैं, और किसी भी एक पंख के बिना वह उड़ नहीं पाएगा। वास्तव में तो कर्म बिना भक्ति के नहीं हो सकते और भक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। सच्चा आंतरिक ज्ञान वही होता है जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि भगवान् ही सर्वोत्तम प्राप्तव्य तत्त्व हैं। जिसे यह बात नहीं समझ आती उसके लिए तो वेदों और शास्त्रों का अध्ययन भी वृथा है। वह सब अध्ययन फिर केवल सूचना-मात्र ही बनकर रह जाता है। सत्ता के प्रत्येक भाग का जानने का अपना तरीका होता है। बुद्धि अपने तरीके से जानती है, हृदय अपने तरीके से जानता है। इनमें हृदय के द्वारा जानने का तरीका अधिक श्रेष्ठ है। जब हृदय में समझ में आ जाता है तब व्यक्ति के मन में भक्ति आती है। ये बातें गीता में अभी प्रकट रूप से सामने नहीं आई हैं। परन्तु धीरे-धीरे गीता इन विषयों में प्रवेश कर रही है। यहाँ यह बता ही दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कर्म किये बिना रह ही नहीं सकता। और कर्मों से संन्यास तो एक मनोवैज्ञानिक भाव है। अतः व्यक्ति कर्मों को यज्ञ, तप और दान के रूप में करता है। अर्थात् व्यक्ति यज्ञ के रूप में कर्म करता है, अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित कर के तप स्वरूप कर्म करता है, और अपनी समस्त चेष्टा, अपने समस्त कर्म भगवान् को दान कर देता है। इसलिए जिसे अनुभव हो चुका है वह तो जानता है कि वास्तव में ज्ञानयोग के द्वारा जिस पद की प्राप्ति होती है वही पद योग मार्ग पर चलने पर प्राप्त होता है। उसके लिए इन दोनों में कोई अन्तर नहीं होता। परन्तु दोनों की सच्ची परिणति तब होती है जब ये दोनों भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। तब ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों ऊपर उठते हैं। जब व्यक्ति पैसे कमाने, पेट पालने या अन्य किसी निहित हेतु से कोई कर्म करता है, तब इसका कोई अधिक मूल्य नहीं होता। कर्मों का वास्तविक मूल्य तो भक्ति के आने पर ही होता है। भाव के बिना या फिर प्रेम या भक्ति के बिना तो कर्म एक प्रकार का बोझ है, जुआ है। इन सब बातों का वर्णन छठे अध्याय में किया गया है। उसके बाद तो गीता का विकासक्रम अद्भुत रूप ले लेगा और अधिकाधिक गूढ़ तत्त्वों का निरूपण होगा।
परंतु अभी तो गीता यहाँ तक पहुँची है कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म देखता है वही सच्चे रूप में देखता है, और वही कर्म-बंधन से छूट जाता है। जो व्यक्ति अहंवश कर्म न कर के भगवान् के निमित्त कर्म करता है उसके कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, वे तो अकर्म के रूप में ही होते हैं। परंतु जो व्यक्ति बाहरी रूप से तो कोई कर्म नहीं करता परन्तु उसके विचार, भावनाएँ सब उस विषय में लिप्स हैं तो बाहरी अकर्म में भी वह घोर कर्म में लिप्त होता है। इसी बात का गहन निरूपण अठारहवें अध्याय में 'त्याग और संन्यास' के बीच के अन्तर में आएगा। कर्मों को जो चीजें दूषित करती हैं वे हैं कामनाएँ और इच्छाएँ। इसलिए कामनाओं और इच्छाओं का त्याग करना होगा न कि कर्मों का और वही सच्चा संन्यास है। जैसे कि, प्रेम में यदि स्वार्थ आ जाता है, तो व्यक्ति को उस स्वार्थ का त्याग करना होगा न कि प्रेम का। इसलिए कर्म में, प्रेम में या फिर अन्य किसी भी चीज में जो निम्न चीजें घुस जाती हैं उनका त्याग करना होता है न कि स्वयं उस चीज का, अन्यथा जीवन में भगवान् की अभिव्यक्ति ही नहीं हो पाएगी। संभव है कि किसी आत्मा-विशेष का अभिव्यक्ति से सरोकार न हो, और उसका उद्देश्य पार्थिव अभिव्यक्ति से छूट निकलना हो। परंतु एक सिद्धांत बनाकर इसे सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। इसीलिए गीता में दिव्य कर्मी के लक्षण बताए हैं कि वह सभी कर्मों को करता है परंतु उन्हें परमात्मा के निमित्त करता है। उसके सभी कर्म समर्पित होते हैं। इसलिए उसके कर्म उस पर बाध्यकारी नहीं होते।
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ।। ७।।
७. जो योगयुक्त है, जो विशुद्ध चित्त है, जिसने अपने आप पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, जिसका आत्मा समस्त भूतों का आत्मा हो गया है, वह कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता।
वह जानता है कर्म उसके नहीं हैं, अपितु प्रकृति के हैं और ठीक इसी ज्ञान के द्वारा वह मुक्त हो जाता है; उसने कर्मों का संन्यास कर दिया है, वह कोई कर्म नहीं करता, यद्यपि कर्म उसके द्वारा संपन्न किये जाते हैं, वह आत्मा हो जाता है, ब्रह्मभूत हो जाता है, वह सृष्टि के समस्त प्राणियों को उसी एक 24 स्वतः विद्यमान सत्ता के व्यक्त रूपों, भूतानि, के रूप में और स्वयं अपनी सत्ता को उन अनेक व्यक्त रूपों में से एक के रूप में देखता है, वह उन सब 'भूतानि' के समस्त कर्मों को उनकी व्यष्टिगत प्रकृति के द्वारा कार्य करती वैश्व-प्रकृति के विकासमात्र के रूप में देखता है और स्वयं अपने कर्मों को भी उसी वैश्व-क्रिया' के ही एक अंश के रूप में देखता है।
अभी तो भगवान् अर्जुन को अपनी परंपरा से सांख्य आदि के विषयों में जो बातें उसने सुन रखी हैं, उन्हीं को बता रहे हैं क्योंकि बिना तैयारी के ही किसी को गूढ़ तत्त्व की बातें नहीं बताई जा सकतीं। और जो बातें बताई जा रही हैं उनका अभी सही-सही निरूपण और समन्वय साधित नहीं किया गया है। इसीलिए यदि गहन दृष्टि से देखा जाए तो जो बात अभी बताई जा रही है वह तो व्यावहारिक रूप में की ही नहीं जा सकती। इसमें विरोधाभास यह है कि जब व्यक्ति अक्षर पुरुष की शांति में चला जाता है तब फिर वह कर्म कैसे कर सकता है, उस शांति में जाने पर कर्म किसलिए और कैसे होंगे। ये दोनों बातें बिल्कुल असंगत हैं। इस असंगतता का बाहरी स्तर पर समाधान नहीं किया जा सकता। परन्तु गीता में यह रहस्य अन्तर्निहित है कि ये दोनों ही एक साथ किये जा सकते हैं क्योंकि गीता में पुरुषोत्तम तत्त्व भी अन्तर्निहित है। परन्तु चूँकि अभी उस तत्त्व को विकसित नहीं किया गया है इसलिए जब तक इस सब का प्रकटन नहीं हो जाता तब तक इस विषय पर पूरा प्रकाश नहीं आ सकता और यह विरोधाभास की-सी स्थिति चलती रहती है।
नैव किश्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्नन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन् ।। ८ ।।
प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ।। ९।।
८-९. निष्क्रिय निर्व्यक्तिक (निर्गुण) ब्रह्म के साथ युक्त मनवाला, पदार्थों के तत्त्व को जाननेवाला मनुष्य देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, मल-मूत्र त्याग करता हुआ, हाथों से किसी वस्तु को ग्रहण करता हुआ, आँखें खोलता हुआ, आँखें बंद करता हुआ भी ये केवल इन्द्रियाँ हैं जो अपने विषयों पर क्रिया कर रही हैं ऐसी धारणा करता है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ऐसा मानता है।
...वह जानता है कि यह वह स्वयं नहीं है जो कर्मशील है, अपितु प्रकृति के त्रिगुण हैं।... वह स्वयं अक्षर अविकार्य आत्मा में सुप्रतिष्ठित होने के कारण त्रिगुण की पाश से परे त्रिगुणातीत हो जाता है; वह न सात्त्विक रहता है, न राजसिक, न तामसिक; उसके कर्मों में प्रकृतिगत गुणों और धर्मों के जो परिवर्तन होते रहते हैं, प्रकाश और सुख, कर्मण्यता और शक्ति, विश्राम और जड़ता रूपी इनका जो छन्दोबद्ध खेल होता रहता है उन्हें वह निर्मल और अविकल भाव से देखता है।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।। १०।।
१०. जो मनुष्य आसक्ति का परित्याग कर के कर्मों को ब्रह्म के ऊपर स्थापित (या प्रतिष्ठित) कर के करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता जिस प्रकार जल से कमल का पत्र लिस नहीं होता।
---------------------------------
' यही गीता की संपूर्ण शिक्षा नहीं है; क्योंकि यहाँ तक केवल अविकार्य आत्मा या पुरुष, अक्षर ब्रह्म का और उस प्रकृति का ही विचार या प्रतिप्रादन है जो विश्व का कारण है, अभी तक ईश्वर का, पुरुषोत्तम का प्रतिपादन स्पष्टतः नहीं किया गया है, यहाँ तक केवल कर्म और ज्ञान का ही समन्वय हुआ है, किन्तु अभी तक, कुछ संकेतमात्र किये जाने पर भी, भक्ति के उस परमोच्च तत्त्व का प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ है जो आगे चलकर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है; यहाँ तक केवल एक अकर्ता पुरुष और अपरा प्रकृति की ही बात कही गयी है, किन्तु अभी तक त्रिविध पुरुष और द्विविध प्रकृति के भेद को प्रकट नहीं किया गया है। यह सही है कि ईश्वर का उल्लेख आया अवश्य है, परंतु उनके आत्मा और प्रकृति के साथ संबंध को सुनिश्चित रूप से नहीं बताया गया है। प्रथम छः अध्याय समन्वय को केवल उतनी ही दूरी तक ले जाते हैं जितना कि इन अत्यंत महत्त्वपूर्ण सत्यों की सुस्पष्ट व्याख्या तथा इनके निर्णायक समावेश के बिना ले जाया जा सकता है और जब इन सत्यों का प्रवेश होगा तो वे इन पूर्व-साधित समन्वयों को, बिना उनका बहिष्कार किये. आवश्यक रूप से विस्तृत और संशोधित कर देंगे।
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि ।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ।। ११ ।।
११. अतः निष्काम कर्मयोगी आसक्ति का परित्याग कर के आत्मशुद्धि के उद्देश्य से शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा अथवा केवल इन्द्रियों के द्वारा भी कर्म किया करते हैं।
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥
१२. जो ब्रह्म के साथ युक्त है वह मनुष्य कर्मों के फलों में आसक्ति का परित्याग कर के ब्रह्म में आनन्दमयी-स्थिति रूप शान्ति को प्राप्त करता है; परन्तु जो ब्रह्म के साथ युक्त नहीं है वह फल में आसक्त होता है और (सकाम भाव से कर्म कर के) उस कर्म से बद्ध हो जाता है।
इस लंबे पथ पर प्रथम सोपान है अपने सभी कर्मों को अपने में तथा जगत् में विद्यमान भगवान् को यज्ञ-रूप से अर्पित करना। यह मन तथा हृदय का भाव है जिसे अपनाना तो कठिन नहीं, परंतु जिसे पूर्ण रूप में सच्चा एवं व्यापक बनाना अत्यंत कठिन है। दूसरा सोपान है अपने कर्मों के फल में आसक्ति का परित्याग; क्योंकि यज्ञ का एकमात्र सच्चा, अवश्यम्भावी तथा सर्वथा अभीष्ट फल एकमात्र आवश्यक वस्तु - यही है कि हमारे भीतर भागवत् उपस्थिति एवं भागवत् चेतना तथा शक्ति प्रकट हो और यदि वह प्राम हो जाए तो बाकी सब कुछ स्वयमेव प्राप्त हो जाएगा। यह हमारी प्राण सत्ता, हमारे काम-पुरुष और हमारी काम-प्रकृति की अहंपरक इच्छा का रूपांतर है, और यह पहले सोपान से कहीं अधिक कठिन है। तृतीय सोपान है केंद्रीय अहंभाव तथा कर्तृत्व के अहंकार से भी छुटकारा प्राप्त करना। यह सभी से कठिन रूपान्तर है और यदि पहले दो सोपानों पर कदम न उठा लिये गए हों तो इसे पूर्णतया सम्पन्न नहीं किया जा सकता। पर वे प्रारम्भिक सोपान भी तब तक संपन्न नहीं हो सकते जब तक रूपान्तर की इस गति को सफल बनाने के लिये तीसरा सोपान प्रारम्भ नहीं हो जाता और अहंभाव का विनाश कर कामना के स्वयं मूल का ही उन्मूलन नहीं कर देता।
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ।। १३।।
१३. जिसने अपनी प्रकृति को पूरी तरह संयत किया है ऐसा देहधारी जीव (पुरुष) समस्त कर्मों का मन से (भीतर से न कि बाहर से) संन्यास कर के न स्वयं करता हुआ न किसी से कराता हुआ इस नौ द्वार वाले नगर (देह) में सुखपूर्वक स्थित होता है।
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।। १४।।
१४. प्रभु न तो लोक के कमाँ की सृष्टि करते, और न कर्तापन के भाव की सृष्टि करते हैं और न कर्मों के उनके फलों के साथ संबंध की सृष्टि करते हैं: प्रकृति ही इन चीजों का प्रवर्तन करती है।
--------------------------------------
अपने आप में यह विचार प्रकृति की यांत्रिक नियति और आत्मा अथवा पुरुष को पूर्ण उदासीनता और अनुत्तरदायित्व के सिद्धांत के निष्कर्ष तक ले जा सकता है, परंतु गोता इस अपूर्ण विचार की भूल का निवारण पुरुषोत्तम-तत्त्व के अपने प्रकाशमान परमेश्वरवादी विचार के द्वारा करती है। गीता यह स्पष्ट कर देती है कि अंततः यह प्रकृति नहीं है जो अपने कर्मों को यंत्रवत् नियत करती हो, अपितु उन पुरुषोत्तम का संकल्प है जो प्रकृति को प्रेरित करता है; जिन्होंने धार्तराष्ट्रों को पहले से ही मार रखा है, अर्जुन जिनका मानव-यंत्र मात्र है, वे विश्वात्मा परात्पर परमेश्वर ही प्रकृति के समस्त उद्यम या कर्मों के स्वामी हैं। निर्व्यक्तिक में कर्मों का आधान करना तो कर्तृत्व-अभिमान से छुटकारा पाने का एक साधन मात्र है, पर हमारा लक्ष्य तो है अपने समस्त कर्मों को सर्वलोकमहेश्वर के अर्पण करना।
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।। १५।।
१५. यह सर्वव्यापी निर्व्यक्तिक आत्मा न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है और न पुण्य को ही ग्रहण करता है: अज्ञान से ज्ञान आवृत्त है इससे जीव मोहग्रस्त हो जाते हैं।
अक्षर ब्रह्म इस द्वन्द्वमय विक्षुब्ध निम्न प्रकृति के ऊपर आत्मा के क्षितिज में विराजमान है, जो कि निम्न प्रकृति के पाप से और पुण्य से अछूता रहता है, वह न तो हमारे पाप के बोध को और न ही हमारे मिथ्याभिमान अथवा दंभ को स्वीकार करता है, इस (निम्न प्रकृति) के हर्ष और शोक से अस्पृश्य रहता है, हमारी सफलता के हर्ष और विफलता के शोक के प्रति उदासीन रहता है, वह सबका स्वामी है, प्रभु है, विभु है, स्थिर, समर्थ और शुद्ध है, सबमें सम है. प्रकृति का मूल है, हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष कर्त्ता नहीं परंतु प्रकृति और उसके कर्मों का साक्षी है, वह हम पर कर्त्ता होने के भ्रम को आरोपित नहीं करता, क्योंकि यह भ्रम तो इस निम्न प्रकृति के अज्ञान का परिणाम है। परन्तु इस मुक्ति, प्रभुता और विशुद्धता को हम देख नहीं पाते; हम प्रकृतिगत अज्ञान के कारण विमूढ़ हुए रहते हैं जो कि हमारे अन्दर ब्रह्म के सनातन आत्मज्ञान को हमसे छिपाये रहता है।
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ।। १६ ।।
१६. अवश्य ही, जिनमें वह अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उनके भीतर वह ज्ञान सूर्य के समान उस परम् आत्मा को प्रकाशित कर देता है।
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्भूतकल्मषाः ।। १७।।
१७. अपनी विवेकशील बुद्धि को 'उस' परब्रह्म की ओर मोड़कर, अपनी संपूर्ण सचेतन सत्ता को 'उस' की ओर प्रवृत्त कर के, 'उसे' ही अपना संपूर्ण उद्देश्य और अपनी श्रद्धा-भक्ति का एकमात्र लक्ष्य बनाकर, ज्ञान के जल (समुद्र) के द्वारा जिनकी निम्न मानवता के समस्त पाप धुल गये हैं वे उस पद को प्राप्त होते हैं जहाँ से उन्हें लौटना नहीं होता।
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।। १८ ।।
१८. ज्ञानी ऋषि विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चाण्डाल में समान दृष्टि रखनेवाले होते हैं।
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ।। १९।।
१९. जिनका मन समता में स्थित है उन्होंने यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए ही सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली है; क्योंकि सम ब्रह्म निर्दोष है, इसलिये (जो समता में स्थित हैं) वे ब्रह्म में निवास करते हैं।
------------------------------------------------
' ऋग्वेद में सत्य की धाराओं का इस रूप में वर्णन है कि वे जल या धाराएँ जिन्हें पूर्ण ज्ञान है, वे जल जो दिव्य सूर्यालोक से परिपूर्ण हैं... जो यहाँ अलङ्कार हैं, वे वहाँ (वेदों में) मूर्त या ठोस प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ।। २०॥
२०. जो प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित न हो और अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर दुःखित न हो, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मोह से रहित है वह ब्रह्म का ज्ञाता है, ब्रह्म में ही स्थित है।
व्यक्ति निष्काम कर्म करता है या नहीं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है समता। यदि व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से विचलित होता है तो इसका अर्थ है कि अभी वह कामना से मुक्त नहीं हुआ है। अतः समता एक उपलब्धि भी है और कसौटी 3 hat pi क्योंकि निष्कामता, निर्लिसता आदि की जिन स्थितियों का वर्णन किया गया है वे सब तो आन्तरिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ हैं, इसलिये इनकी कसौटी है समता। यदि समता नहीं है तो वह इस बात का अचूक प्रमाण है कि ये स्थितियाँ अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। समता तामसिक, राजसिक और सात्त्विक प्रकार की होती है। परन्तु गीता जिस समता की बात करती है वह है ब्रह्म के साथ एक होने पर आने वाली समता, जो कि व्यक्ति की आत्मा के पूरे भाव, उसकी पूरी स्थिति को ही बदल देती है। आरंभ में तो वह समता केन्द्रीय चेतना में आती है और धीरे-धीरे ही वह सत्ता के अन्य भागों में भी प्रवेश करती है। आरंभ में एकाएक ही सभी भागों में समता नहीं आ जाती। और जड़-भौतिक भाग में तो जब तक पूर्ण रूपांतर साधित नहीं हो जाता तब तक असमता कभी भी प्रवेश कर सकती है।
आत्मज्ञान, निष्कामता, निर्वैयक्तिकता, आनन्द, प्रकृति के गुणों से मुक्ति, ये सब जब अंतर्मुख, अपने-आप में आत्मलीन और निष्क्रिय हों तो इन्हें समत्व की कोई आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि वहाँ उन पदार्थों का परिज्ञान ही नहीं जिनमें समता और असमता का द्वन्द्व उत्पन्न होता है। परन्तु ज्यों ही आत्मा प्रकृति के कर्म के बहुत्वों, व्यक्तित्वों, विभेदों और विषमताओं का संज्ञान लेकर उन पर कार्य करने लगती है त्यों ही अपने मुक्त स्वरूप के इन अन्य लक्षणों को वह अपने इस प्रकट लक्षण समत्व के द्वारा कार्यान्वित करती है।... इसीलिए गीता में कर्मयोग के जो तत्त्व बतलाये गये हैं उनमें समत्व को इतना अधिक महत्त्व दिया गया है, वह जगत् के साथ मुक्त आत्मा के मुक्त सम्बन्ध को जोड़नेवाली ग्रंथि है।
समत्व ही अभीप्सु का लक्षण और कसौटी है। जहाँ कहीं जीव में असमता है वहाँ प्रकृति के गुणों की असमान क्रीड़ा गोचर होती है, वहाँ गोचर होते हैं कामना का वेग, व्यक्तिगत इच्छा, संवेदना या कर्म की क्रीड़ा, हर्ष और शोक की क्रिया या फिर वह उद्विग्न या उद्वेगजनक आनन्द की क्रिया जो सच्चा आध्यात्मिक आनन्द नहीं होता अपितु एक प्रकार की मानसिक तृप्ति होती है जो अपने क्रम में अनिवार्य रूप से मानसिक अतृप्ति रूपी प्रतिरूप या प्रतिक्रिया भी साथ लगाए रखती है। जहाँ कहीं जीव के भाव को असमानता है वहाँ-वहाँ ज्ञान से विचलन होता है, सर्वालिंगनकारी और सर्वसमन्वयकारी ब्रह्म की एकता में और चराचर जगत् के एकत्व में दृढ़-प्रतिष्ठ बने रहने का अभाव होता है। अपने समत्व के द्वारा अपने कर्म के मध्य में भी कर्मयोगी यह जानता है कि वह मुक्त है।
परन्तु समता आना आसान नहीं है। श्रीअरविन्द यहाँ भिन्न-भिन्त्र प्रकार की समता की बात करेंगे परन्तु गीता जिस समता की बात करती है, वह एक पूर्ण स्थिति है जो कि व्यक्ति की आत्मा की स्थिति ही बदल देती है। यह समता आंतरिक होती है। समता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति पत्थर के समान हो जाए और उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया जाए, वह किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया न करे। यह समता नहीं, यह तो जड़ता है। ब्रह्म के साथ एकत्व स्थापित होने पर जो समता आती है वही सच्ची समता है, अन्यथा भगवान् अर्जुन को यह कैसे कह सकते हैं कि 'समता रख और अपने शत्रुओं को मार डाल।' सामान्यतः समता का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ लगाया जाता है उसमें तो अर्जुन का युद्ध करने का और अपने शत्रुओं को मार डालने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, क्योंकि उस समता की धारणा में तो उसे युधिष्ठिर और दुर्योधन को समान दृष्टि से ही देखना चाहिये, पर ऐसा करना मूढ़ता ही होती। समता एक बहुत गहरी स्थिति है और इसे समझाने के लिए श्रीअरविन्द यहाँ इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। समता से ही व्यक्ति की परीक्षा होती है। यदि व्यक्ति संसार को त्याग कर जंगल में चला जाए और किसी से कोई मतलब नहीं रखे तब शांत, निर्लिप्त और उदासीन बने रहने में विशेष कोई समस्या ही नहीं बचती। परंतु समता की परीक्षा तो तब होती है जब परिस्थितियाँ विषम या विपरीत हों। तब यदि व्यक्ति उद्विग्न होकर अपना संतुलन खो बैठे तो इसका अर्थ है कि समता अभी तक स्थापित नहीं हुई है।
अपने स्वरूप और अपने समावेशन में उच्च और सार्वभौम जिस समत्व का निर्देश किया गया उसका आध्यात्मिक स्वभाव ही इस विषय में गीता के उपदेश को विशिष्टता प्रदान करता है। अन्यथा समत्व का मात्र इस रूप में उपदेश कि यह अपने आप में मन, भावनाओं और स्वभाव की एक अत्यंत वांछनीय अवस्था है जिसमें पहुँचकर हम मानव-दुर्बलता के ऊपर उठ जाते हैं, किसी भी प्रकार अकेली गीता की ही कोई विशिष्टता नहीं है। समत्व को दार्शनिक आदर्श और साधु-महात्माओं के स्वभाव के लक्षण के रूप में सदा ही सराहा गया है। निःसंदेह गीता इस दार्शनिक आदर्श को लेती अवश्य है परंतु उसे बहुत दूर ऐसे उच्च प्रदेशों में ले जाती है जहाँ हम अपने-आपको अधिक विशाल और विशुद्ध वातावरण में श्वास लेता पाते हैं। आत्मा की वैरागी अथवा दार्शनिक स्थिति तो भावावेगों के भँवर और कामनाओं की हलचलों से निकलकर स्वयं भगवान् की (न कि देवताओं की) उनकी परम् आत्म-प्रभुत्वपूर्ण शान्ति और आनन्द की अवस्था तक आरोहण में पहली या दूसरी सीढ़ी है। तापसी (स्टोइक) समता आचरण को अपनी धुरी या केंद्र-बिंदु बनाकर अपने आप को कठोर सहिष्णुता के द्वारा आत्म-प्रभुत्व पर प्रतिष्ठित करती है; इससे अधिक सुखकर और शान्त प्रकार की दार्शनिक समता ज्ञान के द्वारा, अनासक्ति के द्वारा और हमारे प्राकृत स्वभावसुलभ विक्षोभों से ऊपर उठी हुई उच्च बौद्धिक उदासीनता के द्वारा आत्म-प्रभुत्व प्राप्त करने को 9 अधिक वरीयता प्रदान करती है, इसी को गीता ने कहा है 'उदासीनवद् आसीनः।' इसके अतिरिक्त एक धार्मिक या ईसाई प्रकार की समता भी है जिसका स्वरूप है भगवदिच्छा के सामने सदा नत होकर, घुटने टेककर झुके रहना या साष्टांग प्रणिपात के द्वारा भगवान् की इच्छा को सिर माथे चढ़ाना। दिव्य शान्ति की ओर जाने के ये तीन साधन तथा सोपान हैं - वीरोचित सहनशीलता, विवेकपूर्ण या साधु समान उदासीनता और धर्मनिष्ठ समर्पण, अर्थात् तितिक्षा, उदासीनता, नमस् अथवा नति। गीता इन सभी को अपनी व्यापक समन्वयात्मक रीति से समाविष्ट कर लेती है और अपनी ऊर्ध्व आत्म-गति में उन्हें घुला-मिला लेती है, परंतु वह इनमें से प्रत्येक को एक गहनतर मूल, एक व्यापकतर दृष्टिकोण, एक अधिक सार्वभौमिक और सर्वातीत अर्थ प्रदान करती है। क्योंकि चारित्रिक लक्षणों से परे, बुद्धि की दुष्कर स्थिति से परे और भावावेगों के तनाव या दबाव से परे यह प्रत्येक को आत्मा के मूल्य और उसकी आध्यात्मिक सत्ता की शक्ति प्रदान करती है।
तीन प्रकार की समता बताई गई हैं- तामसिक, राजसिक और सात्त्विक। मनुष्यों में मानसिक चेतना के कारण ही समता-असमता का विषय उठता है अन्यथा पशुओं में समता-असमता का कोई विषय ही नहीं होता क्योंकि वे तो प्रकृति के आधीन हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रिया करते रहते हैं। उनमें समता जैसी कोई मनोवैज्ञानिक परिकल्पना होती ही नहीं। मनुष्य अपनी बुद्धि के सहारे समता की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके तीन सोपान है -पहले में तो शरीर-संबंधित व्याधियाँ स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य, सदर्दी-गर्मी, पीड़ा-आराम आदि - मनुष्य को अस्थिर कर देती हैं। ग्रीस में स्टोइक दार्शनिक थे जिनका कहना था कि हमें ऐसा कठोर हो जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार की यातना, संकट, सर्दी-गर्मी कुछ भी हों परन्तु हम उनसे प्रभावित न हों। हमारे शास्त्रों में भी ऐसे तपस्वियों का वर्णन है जो गर्मी के अन्दर सूरज की तपती धूप में बैठ जाते थे और सर्दियों में सारे कपड़े निकाल कर ठंडे पानी में बैठ जाते थे। इस तरीके से वे शरीर को ऐसा तैयार कर लेते थे कि वह सर्दी-गर्मी, दुःख-दर्द आदि से विचलित न हो सके। इस पद्धति से शरीर में दृढ़ता लाकर उस पर विजय प्राप्त कर समता लाने का प्रयास किया जाता है और बहुत-सी असमानताएँ जिनसे शरीर विचलित होता है उनको नियंत्रित किया जाता है। जब व्यक्ति शरीर पर नियंत्रण करता है तो वह अपने प्राण को भी- जो कि कुछ हद तक उसके दुःख-दर्द आदि से प्रभावित होता है - कुछ हद तक वश में कर सकता है। इस प्रकार समता की ओर चलने का यह एक तरीका है। इसमें व्यक्ति के अन्दर दुःख-दर्द, आराम-तकलीफ आदि को सहन करने की क्षमता आ जाती है और वह विचलित नहीं होता। इस स्थिति को तितिक्षा कहते हैं, जिसमें भौतिक प्राण और शरीर में समता आ जाती है। दूसरी स्थिति है, भावात्मक समता की। उदाहरण के लिये, यों तो दुनिया में कितने ही व्यक्तियों की मृत्यु होती रहती है, और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता परन्तु जैसे ही हमारे किसी प्रिय मित्र या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु का समाचार मिलता है तो हम विचलित हो उठते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी भावनाओं को गहरी चोट पहुँचाती हैं। हमारा यदि किसी के प्रति बहुत भाव है और उसके साथ कुछ बुरा घटित हो जाए या उसके बारे में कोई कुछ भला-बुरा कह दे तो हम तुरन्त विचलित हो उठते हैं। और मनुष्य के लिए इस प्रकार विचलित हो उठना बिल्कुल स्वाभाविक ही है। ये सब भावनात्मक क्रियाएँ हृदय के द्वारा होती हैं। ऐसे में यदि हमारे अंदर यह भाव हो कि श्रीमाँ विद्यमान हैं और वे हमसे जितना प्रेम करती हैं उतना दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यदि अन्य कोई दूसरा व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तो उसके माध्यम से भी वे ही हमसे प्रेम करती हैं। यदि हमारा किसी के प्रति मोह भी है, तो उसके पीछे भी श्रीमाँ ही उसके माध्यम से हमसे प्रेम कराती हैं। और वे इतनी सर्वसमर्थ और दयालु हैं कि वे जो कुछ भी करती हैं, वह सब हमारे भले के लिए ही करती हैं। अतः यदि श्रीमाँ के प्रति ऐसी गहरी भावना हो तो उस भाव के प्रभाव से और उनसे प्रेम के कारण हमारे अन्दर समता अपने-आप ही आ जाएगी। और एक बार यह भाव आ जाने पर व्यक्ति किसी भी चीज से विचलित नहीं होता। इसीलिये श्रीअरविन्द आश्रम में श्रीमाताजी सभी के साथ उसकी आवश्यकतानुसार व्यवहार करती थीं, उन्हें भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियाँ दिया करती थीं, भिन्न-भिन्न साधन-संसाधन प्रदान करती थीं। परंतु प्रत्येक साधक गहरे रूप से संतुष्ट था और यह भाव रखता था कि श्रीमाताजी उससे विशेष रूप से प्रेम करती हैं और उसकी आत्मा के लिए जो सर्वोत्तम है वही व्यवहार करती हैं।
इस प्रकार यह समर्पण का भाव, अपने इष्ट के प्रति प्रेम का भाव भावनात्मक समता ले आता है। जब व्यक्ति यह विश्वास करता है कि भले ही उसे समझ में न आ रहा हो और भले ही वह क्रिया उसे बुद्धि से अनुकूल न लग रही हो तो भी उसके गुरु ने, इष्ट ने जो भी किया है वह तो अच्छे-से-अच्छा ही है और उसके भले के लिये ही है। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तब कैसी भी प्रिय-अप्रिय घटना क्यों न हो, व्यक्ति विचलित नहीं होता और उसमें धीरे-धीरे समता आती जाती है।
इस प्रकार पहली अवस्था में व्यक्ति तितिक्षा के द्वारा अपने भौतिक भागों में समता लाता है। न तो वह दुःख-दर्द के स्पर्शों से विचलित होता और न ही सुखद स्पर्शों से प्रसन्न हो जाता है। वह शांत भाव से दोनों को समान ही समझता है। और दूसरी अवस्था में व्यक्ति उदासीनता के द्वारा भौतिक और मानसिक द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वह सभी द्वंद्वमय स्पर्शों को समभाव से सहन करता है। उसके बाद है 'नति' अर्थात् भगवदिच्छा के प्रति नत होने के द्वारा, समर्पण के द्वारा अपने भावनात्मक भागों में समता ले आना। इसमें व्यक्ति सभी स्पर्शों को भगवान् की ओर से आते स्पर्शों के रूप में लेता है। दार्शनिक भाव की, बुद्धि की समता में व्यक्ति चेतना के एक ऐसे स्तर पर रहता है जहाँ उसे संसार की निस्सारता दिखाई देती है। उसे सभी घटनाएँ वैसी ही लगती हैं मानो किसी विशाल भूखंड पर कुछ छोटी नगण्य चीजें पड़ी हों जिनके बने रहने या नष्ट हो जाने से व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार व्यक्ति इस भाव में निवास करता है कि यह सारा संसार तो मृत्यु के आधीन है, क्षणभंगुर है, पर हम तो भगवान् के अंश हैं और अपने सच्चे स्वरूप में शाश्वतता में निवास करते हैं। इसलिए इस क्षणिक संसार में ऐसी क्या चीज हो सकती है या फिर ऐसी कौनसी घटना हो सकती है जो हमें विचलित कर सके। तो यह है बुद्धि के सहारे समता लाना। इस प्रकार श्रीअरविन्द तामसिक, राजसिक, सात्त्विक आदि भिन्न-भिन्न प्रकार की समताओं की चर्चा कर रहे हैं। गीता इन सभी को स्वीकार तो करती है क्योंकि ये पथ पर आगे बढ़ने में सहायक हैं, परन्तु जिस समता की वह बात करती है वह तो सुदूर एक विरली स्थिति में ले जाती है। वह समता है परम् प्रभु के साथ ऐक्य के द्वारा आने वाली समता। परम् प्रभु सब कुछ से ऊपर हैं, उन्हें समत्व बनाए रखने के लिए किन्हीं साधनाओं की, किन्हीं मानसिक सुझावों की या अन्य किन्हीं सहारों की आवश्यकता नहीं होती। उनको चेतना अखण्ड होती है और उस चेतना में यदि वे सारे संसार के साथ कठोर से कठोर व्यवहार भी करें या सारे संसार को नष्ट भी कर दें तो भो अपनी समता से नहीं डिगते। श्रीअरविन्द कहते हैं कि गीता इन सारी समताओं का वर्णन करती है और अंततः परम् प्रभु की ओर ले जाती है। इस तरीके की समता केवल भगवान् के साथ ऐक्य से ही प्राप्त को जा सकती है। अन्यथा मानसिक, राजसिक या तामसिक प्रकार को समता मानसिक दृष्टिकोण, समर्पण भाव, सहनशीलता आदि के सहारे स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिनमें एक सीमा से अधिक दबाव सहने की क्षमता नहीं होती जिससे उनके भंग होने की आशंका रहती है। प्रयत्न कर के भावात्मक, मानसिक और शरीर की सहनशीलता आदि से जो समता लाई जाती है वह अधिक समय तक टिक नहीं सकती। परन्तु गीता की समता तो सहज और पूर्ण स्थिति है।
गीता इसी समता की ओर इंगित करती है, जो कि अन्तरात्मा का सारा भाव ही परिवर्तित कर देती है। व्यक्ति का सारा कार्य-व्यवहार ही बदल जाता है और वह किसी भी प्रकार विचलित नहीं होता। और वह जिसके साथ जैसा व्यवहार करना होता है वैसा यथायोग्य व्यवहार करता है। समता के संबंध में ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। बाहरी रूप से इनमें विभेद नहीं किया जा सकता। इनकी कसौटी तो आंतरिक है।
सामान्य मानव जीव अपने प्राकृत-जीवन के सामान्य अथवा अभ्यस्त बखेड़ों में एक तरह का सुख लेता है; और चूँकि वह उनमें सुख लेता है और उस सुख को पाकर वह निम्न प्रकृति की कष्टमय क्रीड़ा को एक स्वीकृति देता है इसलिए यह क्रीड़ा अनवरत चलती रहती है; क्योंकि प्रकृति अपने प्रेमी और भोक्ता, पुरुष, के सुख के हितार्थ और उसके अनुमोदन से ही (क्रीड़ा करती है) उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करती। हम इस सत्य को नहीं पहचान पाते, प्रतिकूल विघ्न-अशांति के प्रत्यक्ष आघात के चलते, शोक, पीड़ा, क्लेश, दुर्भाग्य, विफलता, पराजय, दोष या कलंक, अपमान के संताप के आघात से मन सहमकर पीछे हटता है, वहीं वह उत्कटता से इसके विपरीत और सुखद उत्तेजनाओं - हर्ष, सुख, हर प्रकार की तुष्टियों, समृद्धि, सफलता, जय, गौरव, प्रशंसा - को गले लगाने के लिए उछल पड़ता है, परंतु इससे इस सत्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता कि जीव जीवन में सुख लेता है और यह सुख मन के द्वन्द्वों के पीछे सदा बना रहता है। योद्धा को अपने घावों से शारीरिक सुख नहीं मिलता और न अपनी पराजयों में मानसिक संतोष ही पाता है; परंतु उसे उस रण के देव में पूर्ण आनन्द मिलता है जो उसके लिये जहाँ पराजय और घाव लाता है वहीं उसके साथ-ही-साथ दूसरी ओर विजय का हर्ष भी लाता है, वह पराजय और घावों की आशंका को और विजय-हर्ष की आशा को युद्ध के घुले-मिले ताने-बाने के अंग के तौर पर स्वीकार करता है, और उसका यह आनन्द उसे इसमें बनाए रखता है। युद्ध के घाव की स्मृति भी उसे हर्ष और गौरव देती है, पूरा हर्ष और गौरव तो तब होता है जब घाव की पीड़ा का अन्त हो जाता है। परन्तु प्रायः पीड़ा के रहते हुए भी ये उपस्थित रहते हैं और पीड़ा वास्तव में इनका पोषण करती है। पराजय उसके लिए अधिक बलवान् शत्रु के अदम्य प्रतिकार करने का हर्ष और गर्व रखती है, अथवा यदि वह हीन कोटि का योद्धा हो तो उसे द्वेष और प्रतिशोध की भावनाओं से भी एक प्रकार का गर्दा (darker) और क्रूर सुख मिलता है। इसी प्रकार आत्मा भी हमारे जीवन की प्राकृत क्रीड़ा में सुख लेती रहती है।
गीता तथा हमारे अन्य शास्त्र आदि यही कहते हैं कि प्रकृति ऐसा कुछ नहीं करती जिसमें हमारी सच्ची सत्ता, हमारी अन्तरात्मा आनंद न लेती हो। हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति अपनी मनचाही करती है, और केवल दो घड़ी का आनन्द देती है उसके बाद लंबी तकलीफ देती है अतः यह जीवन दुःखमय और कष्टमय है। परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दुःखों और कष्टों में भी हमारा कोई भाग आनन्द ले रहा होता है इसीलिए ये चीजें हमारे साथ घटित होती हैं। चाहे कोई कितनी भी तकलीफ में क्यों न हो परन्तु इस गूढ़ आनंद के कारण ही कोई भी अपनी मृत्यु नहीं चाहता। उसे इस सब प्रपंच में एक गूढ़ आनंद अनुभव होता है।
यहाँ श्रीअरविन्द यह समझा रहे हैं कि अन्तरात्मा कोई इतनी छिछली और तुच्छ नहीं है कि वह जीवन की छोटी-छोटी प्रगति, हर्ष, सुख आदि में आनन्द लेती हो। ये सब तो उसके लिए खेल-मात्र हैं। जैसे जो खिलाड़ी केवल जीतने में ही आनन्द लेता हो और हार जाने पर विक्षुब्ध होकर मरने की तैयारी करता हो, वह तो कभी अच्छा खिलाड़ी हो ही नहीं सकता। हार-जीत तो केवल ऊपरी बातें हैं, गहराई में तो उसको उसमें आनंद आता है। इसी प्रकार हमारी अंतरात्मा सभी कुछ में आनंद अनुभव करती है। जय-पराजय, सुख-दुःख, अच्छा-बुरा आदि तो केवल सतही भौतिक, प्राणिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ मात्र हैं जिन्हें हम बहुत हद तक अपने दृष्टिकोण के सहारे बदल सकते हैं। यदि हमारे किसी प्रिय व्यक्ति का देहांत हो जाए तो सामान्य प्रतिक्रिया दुःख और पीड़ा की होती है। पर इसमें यदि व्यक्ति यह मनोभाव अपनाए कि भले ही उसे अपने प्रिय के मर जाने का दुःख है परंतु स्वयं वह व्यक्ति तो जो यंत्रणा वह शरीर में पा रहा था उससे अब छूट चुका है और एक अधिक अच्छी स्थिति में है। जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारी सारी प्रतिक्रिया ही बदल जाती है और जो चीज हमें पहले अत्यधिक पीड़ा दे रही थी वही अब उतनी दुःखद नहीं प्रतीत होती या फिर कुछ हालातों में तो सुखद लगने लगती है। अतः यह सब केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। परंतु अंतरात्मा इन सब द्वंद्वों से अधिक गहरी स्थिति में है और इसीलिये वह दोनों ही परिस्थितियों में समान रूप से सुख लेती है और इसी कारण प्रकृति का यह खेल चलता रहता है। यदि अन्तरात्मा को यह पसंद न हो तो प्रकृति का यह खेल क्षण भर भी नहीं चल सकता। वास्तव में तो प्रकृति अन्तरात्मा की प्रसन्नता के निमित्त ही सारी व्यवस्था करती है। इसलिये जब तक अंतरात्मा को इस सारे प्रपंच में एक गूढ़ आनन्द आता रहेगा तब तक हमारी सभी बाहरी प्रतिक्रियाओं के बावजूद भी यह सब चलता रहेगा।
इसलिये प्रकृति की क्रीड़ाओं से ऊपर उठने के लिए गीता कहती है कि व्यक्ति को पहले साक्षी भाव अपनाना होगा। और जब व्यक्ति साक्षी भाव से चीजों को देखता है तब वह अनुभव करता है कि उसकी अनुमति से ही यह सब प्रपंच चल रहा है। और इसके बाद उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि वह केवल अनुमंता ही नहीं बल्कि इस प्रपंच का भर्त्ता भी है। और भर्त्ता भाव के बाद यह ज्ञात हो जाता है कि वह केवल भर्ता ही नहीं अपितु इसका भोग करने वाला भोक्ता है। और जब व्यक्ति धीर-धीरे ये भाव अपना कर प्रकृति के रहस्य को जान जाता है तो अंत में वह उसके ईश्वरत्व के भाव में भी जा सकता है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि प्रकृति और कुछ नहीं केवल वही करती है जो स्वयं व्यक्ति को अच्छा लगता है। इसलिए गीता की पद्धति के अनुसार यदि व्यक्ति को प्रकृति की अधीनता की अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना हो तो उसे साक्षी, अनुमता, भर्त्ता, भोक्ता, ज्ञाता और ईश्वर आदि भावों से क्रमशः बढ़ना होता है।
जिस दिन व्यक्ति की अंतरात्मा यांत्रिक रूप से प्रकृति की क्रीड़ा के वशीभूत हो सुख-दुःख, राग-द्वेष, प्रसन्नता-अप्रसन्नता, निराशा-उत्तेजना आदि द्वन्द्वों में चलते रहने से ऊब जाती है तब वह साक्षी के भाव से आरंभ कर धीरे-धीरे प्रकृति के ईश्वर भाव तक जा सकती है। परंतु जब तक वह इसमें रस लेती रहती है तब तक कितने भी बाहरी प्रयास किये जाएँ तब भी इन द्वंद्वों से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि इन सबकी कुंजी तो भीतर है।
मन जीवन के प्रतिकूल आघातों से कष्ट और अरुचि के द्वारा पीछे हटता है; यह 'जुगुप्सा' प्रकृति द्वारा आत्म-रक्षा के सिद्धांत को लागू करने हेतु प्रयुक्त की गई युक्ति है, जिससे कि हमारे अतिसंवेदनशील या कमजोर स्नायविक तथा शारीरिक अंग अनावश्यक रूप से सहसा अपने आत्म-संहार का आलिंगन करने के लिए न दौड़ पड़ें। जीवन के अनुकूल स्पर्शों में मन हर्ष लेता है; यह प्रकृति का राजसिक सुख का प्रलोभन है, ताकि जीव के अंदर निहित शक्ति जड़ता और अकर्मण्यता की तामसी प्रवृत्तियों को जीत सके और वह कर्म, कामना, संघर्ष और सफलता की ओर पूरी तरह से प्रवृत्त हो जाए और मन की इन चीजों के साथ आसक्ति के द्वारा प्रकृति के प्रयोजन सिद्ध हो सकें। हमारी गूढ़ आत्मा इस द्वन्द्व और संघर्ष में, यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थिति या आपकाल और संत्रास में भी एक प्रकार का सुख अनुभव करती है, ऐसा सुख जो कि अतीत विपद् को याद करने और पीछे फिरकर देखने में तो उसे पूरा मिलता ही है, पर जिस समय विपद्काल सिर पर हो उस समय भी प्रच्छन्न रूप से पीछे बना रहता है और यहाँ तक कि प्रायः सतह पर आकर संतप्त मन को उसके भावावेग में समर्थन तक करता है। परन्तु जो चीज आत्मा को सचमुच आकर्षित करती है वह है इस संसार का नानाविध द्वन्द्वों से भरा हुआ वह पदार्थ जिसे हम जीवन कहते हैं, जो संघर्ष और कामना के विक्षोभ से, आकर्षण और विकर्षण से, लाभ और हानि से, हर प्रकार के अपने वैविध्य से भरा है। हमारे राजसिक कामनामय पुरुष के लिए एक-समान सुख, संघर्षरहित सफलता और किसी छाया के बिना हर्ष अवश्य हो कुछ काल बाद थकाने वाला, नीरस, और उबाऊ हो जाता है, इसके प्रकाश के सुख को पूरा महत्त्व प्रदान करने के लिए इसे अंधकार को पृष्ठभूमि चाहिएः क्योंकि जो सुख वह खोजता और भोगता है वह ठीक उसी स्वभाव का है, अपने मूलस्वरूप में भी यह सापेक्ष अथवा अपूर्ण होता है तथा अपने विपरीत तत्त्व के बोध और अनुभव पर निर्भर है। मन जो जीवन में सुख लेता है उसका रहस्य है हमारी आत्मा की द्वन्द्वों में रसानुभूति।
हमारे सामने प्रकृति की जो मुख्य समस्या है वह यह है कि हमारी प्रकृति तामसिक और जड़ है। इसलिये जब पहले-पहल जीवन का प्रादुर्भाव हुआ तब उसके संरक्षण के लिये प्रकृति ने अनेक संवेदन काम में लिये। हमारे जीवन में कामनाएँ और भय न होते तो हम कभी भी कोई क्रिया ही नहीं करते। मनुष्य कामनाओं के कारण या फिर भय के कारण क्रिया करते हैं। ये प्रलोभन प्रकृति ने हमारे अन्दर डाल दिये। यदि ये भौतिक संवेदन न होते तो जीवन की रक्षा ही न हो पाती। यदि शरीर में पीड़ा का संवेदन न होता तो शरीर की रक्षा मुश्किल हो जाती। यदि आग में हाथ देने पर जलने का संवेदन न होता और दर्द न होता तो व्यक्ति को पूरा जलने पर भी पता न चलता। उसी प्रकार भूख और जीभ का स्वाद न होता तो कोई भोजन ही न करता। इसलिये यदि प्रकृति लोभ, लालच आदि की क्रिया संलग्न न करती तो जीव नष्ट ही हो जाता। और आत्मा इस धरती पर जिस अभियान के लिए आई है वह पूरा नहीं हो पाता। इसलिये प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो चीजें आत्मा के लिए प्रतिकूल हैं और जिन चीजों से जीव की रक्षा होनी चाहिए वे उसे अप्रिय लगेंगी, खराब लगेंगी और जो अनुकूल होंगी वे अच्छी लगने लगेंगी। जब हमारी मानसिकता विकसित होती है, हमारा मनोवैज्ञानिक ढाँचा विकसित होता है, तब सचेतन रूप से समीकरण में हस्तक्षेप कर हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि जब व्यक्ति अधिक विकसित नहीं होता तब वह जिस देश या जाति में पैदा होता है उसी के भोजन में, उसी के तौर तरीकों में रस लेता है और उन्हें ही सबसे अच्छा मानता है। परंतु ज्यों-ज्यों उसकी चेतना में विस्तृतता आती है, त्यों-त्यों वह केवल अपने ही तौर तरीकों पर आग्रह नहीं रखता अपितु सभी तौर-तरीकों के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है। और धीरे-धीरे इन सबसे ऊपर उठ कर वह सभी में समान रूप से आनंद ले सकता है। इस तरीके की हमारी मनोवैज्ञानिक संरचना बनी हुई है। सारे जीवन का यह खेल इसलिए चलता है क्योंकि इसमें हमारी आत्मा को आनन्द आता है। और सतही तौर पर देखा जाए तो इस खेल में हमारी प्राणिक सत्ता को आनन्द आता है। उसे कभी भी कोई एकरस चीज पसंद नहीं आती। न उसे एकरस सुख पसंद आता है और न उसे एकरस दुःख। उसे तो सदा ही बदलते हुए रंग पसंद आते हैं। एक-समान चीज से वह बहुत ही जल्दी ऊब जाती है। यही मुख्यतया लड़ाई-झगड़ों का कारण है। क्योंकि उसे लड़ाई-झगड़े में भी उतना ही सुख मिलता है जितना कि उसके बाद होने वाले मेल-जोल से। यदि प्राण इन चीजों में रस लेना बंद कर दे तो जीवन की सारी वर्तमान दशा ही बदल जाएगी। वर्तमान में तो हमें इन सतही चीजों में ही आनन्द आता है। परंतु जब हमें इन सतही चीजों में आनन्द आना बंद हो जाता है तब यह सारा खेल, ये सारी चीजें यों लुप्त हो जाती हैं मानो पहले कभी वे थीं ही नहीं। क्योंकि अब हमें किसी दूसरी चीज में आनंद आने लगता है। और जब हमें परमात्मा के आनन्द का स्वाद आ जाता है तब अन्य किसी चीज में अधिक रुचि नहीं रह जाती। परन्तु जब तक हमें परमात्मा का आनन्द नहीं प्राप्त होता तब तक यह आशा नहीं की जा सकती कि हम निम्न सुख को छोड़ सकें। जब तक व्यक्ति को समर्पण में आनन्द नहीं आता, तब तक तो उसकी अपनी इच्छाएँ ही बलवती होती हैं और वह उन्हीं के अनुसार काम करता रहता है। परंतु जब उसे गुरु के प्रति या फिर अपने इष्ट के प्रति समर्पण का आनंद आता है तभी वह अपनी निजी इच्छा को उसके आदेश के अधीन रख सकता है। यदि ऐसा करने में उसे किसी गहरे आनंद की अनुभूति न होती और केवल पोड़ा ही होती तो वह अधिक समय तक उसमें लगा नहीं रह सकता था। व्यक्ति गुरु के प्रति या फिर अपने इष्ट के प्रति तभी समर्पित रह सकता है जब हजारों कष्टों के बावजूद भी उसकी आत्मा को उसमें गहरा आनन्द आता हो। तब उसे गुरु के लिये या फिर अपने प्रेमी के लिए उठाए कष्टों में भी गहरे आनंद की अनुभूति होती है। केवल किसी सिद्धांत के सहारे ऐसा नहीं किया जा सकता। समस्त साधना की सच्ची उपलब्धि यही है कि बाहरी चीजों में सुख बटोरने की बजाय आत्मा को भगवान् में आनन्द आने लग जाए। और हमें जिस चीज में आनंद आता है प्रकृति उसी के अनुरूप व्यवस्था करती है। केवल परम् आनन्द ही है जो अपने-आप को पूर्ण रूप से दे सकता है। केवल आनन्द ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने-आप को अपने प्रेमी के लिए, गुरु के लिए, परमात्मा के लिए पूर्ण रूप से मिटा सकता है। यही जीवन का रहस्य है।
यही साधना का अर्थ है- अपनी चेतना को संवर्धित कर के निम्न चीजों में रस लेने की बजाय अधिकाधिक गहरी चीजों में रस लेना और फिर केवल परमात्मा में ही रस लेना। वेदों में भी विषयों के रस को सोमरस नहीं बताया गया है। जब व्यक्ति को अधिकाधिक परिष्कृत रूप से गहरी चीजों में रस की अनुभूति होती है तब उसे सोम कहते हैं और धीरे-धीरे वह बढ़ने लगता है। और जब सोम बढ़ता है तब उसके प्रभाव से अन्य सभी देवता पुष्ट होते हैं और जब वे पुष्ट होते हैं तब हमें अधिकाधिक अमरत्व की ओर ले जाते हैं। और इस प्रकार यह सारी क्रिया चलती रहती है।
गीता के श्लोक में तो ये बातें इस रूप में नहीं हैं परंतु इस पूरे विषय को समझने के लिये ये सब आवश्यक हैं ताकि पूरा विषय और इससे संबंधित चीजें अधिक अच्छी तरह समझ में आ सकें। वास्तव में तो जो कुछ हो रहा है वह मूलभूत रूप से हमारी अंतरात्मा की, श्रीमाताजी की, जगज्जननी की स्वीकृति से ही हो रहा है। परंतु यदि हमारी गहरी से गहरी सत्ता, हमारी अन्तरात्मा इन निम्न प्रकृति की चीजों में इसी रूप में रस ले रही होती तब तो फिर कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता था। परंतु हमारी सतही सत्ता से अधिक गहरी सत्ताएँ होती हैं - जैसे प्राणिक सत्ता, सौन्दर्यग्राही सत्ता, मनःसत्ता आदि - जो अपना-अपना सन्तोष लेती हैं। हालाँकि इन सब के द्वारा भी अन्तरात्मा ही आनंद लेती है, परंतु परोक्ष प्रयास करता है उससे अधिक संघर्ष और प्रयास ही अपेक्षित होता है।
अधिकांश व्यक्ति जो कि इस स्थिति में रहते हैं उन्हें यदि यह समझाया जाए कि - ये सुख-दुःख तो क्षणिक हैं, चिरस्थायी नहीं हैं, और यह ऐसा नशा है जो चढ़ता-उतरता रहता है, स्थायी उन्मत्तता तो आध्यात्मिक सुख में ही है - तो उन्हें इस बात में कोई रस नहीं आता क्योंकि वे तो विषय-भोग के कीड़े हैं और उसी में सुख लेते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी ही होती है, वे आध्यात्मिकता की बातें तो बहुत करते हैं परन्तु वास्तव में उन्हें प्रकृति की इन्हीं क्रीड़ाओं में रस आता है और इन्हें छोड़ने को वे तैयार नहीं होते, फिर चाहे उनको कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े, वे उसी के अन्दर कीड़े की तरह रेंगते रहते हैं। व्यक्ति का निम्न प्राण कभी भी परमात्मा की ओर जाने को सहमत नहीं होता क्योंकि वह तो प्रकृति के द्वन्द्वों में ही आनन्द लेता है। प्राण को परमात्मा की ओर जाना बहुत अधिक नीरस लगता है। जबकि व्यक्ति अपनी कामनाओं की तुष्टि के लिए जीवन भर जितना घोर प्रयत्न करता है उसकी तुलना में साधना में उसका आधा प्रयत्न भी नहीं होता और व्यक्ति हमेशा के लिए ऊपर उठ जाता है। परन्तु फिर भी वह यह काम करने को तैयार नहीं होता। अधिकांश व्यक्तियों के साथ यही बात है। इसलिए जीवन में विरले ही मनुष्य - जिनकी आत्मा जन्मों-जन्मों से प्रबल हो चुकी है - इससे विरत होकर अपने जीवन को परमात्मा की ओर मोड़ पाते हैं।
इसकी अनिच्छुकता का वास्तविक कारण यह है कि उसे उसके अपने वातावरण से ऊपर उठने और जीवन की एक अधिक असाधारण और अधिक विशुद्ध वायु में साँस लेने के लिए कहा जाता है, जहाँ के आनन्द और शक्ति को वह अनुभव नहीं कर सकता, और जिसकी वास्तविकता तक पर भी उसे मुश्किल से ही विश्वास होता है, जबकि इस निम्नतर गंदी प्रकृति के सुख ही उसके लिए एकमात्र सुपरिचित और स्पर्श करने या भोगने योग्य हैं। और न ही यह निम्नतर संतुष्टि या सुखभोग अपने-आप में कोई बुरी और व्यर्थ की चीज है; अधिक उचित रूप से कहें तो, यह उस तामसिक अज्ञान और जड़ता - जिसके कि उसकी भौतिक सत्ता सबसे अधिक अधीन होती है - में से ऊर्ध्वमुखी विकास की अवस्था है; यह मनुष्य के परम् आत्मज्ञान, शक्ति और आनन्द की ओर क्रमिक आरोहण की राजसिक अवस्था है। परन्तु यदि हम अनन्त काल तक इसी स्तर पर विश्राम करते रहें, जिस स्तर को गीता ने मध्यमा गति कहा है, तो हमारा आरोहण अपूर्ण रह जाता है, आत्मा का विकास अधूरा रह जाता है। जीव का अपनी सिद्धि तक का मार्ग सात्त्विक सत्ता और सात्त्विक प्रकृति से होकर उस तक पहुँचता है जो त्रिगुणातीत है।
प्राण की अवस्था एक राजसिक अवस्था है। भौतिक सत्ता तो निरी तामसिक होती है जो जरा भी तकलीफ उठाना नहीं चाहती और केवल अपने ही सुख-साधन में लगी रहती है। प्राण में उसकी अपेक्षा अधिक विशालता होती है जो दूसरों के सुख-दुःख में भी भाग लेता है और कष्ट आदि सहन करने को तैयार रहता है। परंतु यह राजसिक अवस्था मध्यमा गति है और यदि व्यक्ति इसी पर लम्बे समय तक चलता रहे तो उसका आगे की ओर आरोहण नहीं हो सकता। परन्तु प्राण को अपनी ही चीजों में इतना सुख मिलता है कि वह इन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। जब आत्मा बुद्धि के द्वारा अपना काम करती है तब बुद्धि के दबाव के अन्दर ही वह थोड़ा-बहुत आरोहण कर सकता है अन्यथा तो कदम-कदम पर उन्हीं ढरों में लौट जाने के लिए लालायित रहता है। जैसे कि यदि कोई अनेकों अनुभव प्राप्त कर के एक महात्मा तो बन गया हो तो भी प्राण तो उसमें भी अपनी संतुष्टि लेने का प्रयास करेगा। उसके अंदर प्राण इस प्रकार के भाव उठा देगा कि उसके समान तो कोई दूसरा महात्मा ही नहीं है जिसने उतना भारी त्याग किया हो या फिर तप किया हो। इस प्रकार प्राण अंत तक भी अपना प्रभाव डाले बिना नहीं छोड़ता। यह काम तो केवल कोई महान् आत्मा ही कर पाती है। भले ही व्यक्ति षड् रिपुओं को भी कुछ हद तक जीत ले, परंतु जब तक अहं शेष है तब तक यह भाव जा ही नहीं सकता कि व्यक्ति कुछ विशेष है। और जब तक यह भाव रहता है तब तक तो सभी आसुरिक वृत्तियों के लिए रास्ता खुला होता है। इसलिए जब तक पूर्ण रूपांतर साधित नहीं हो जाता तब तक इसका प्रभाव कभी भी दूषित कर सकता है।
इसलिए इन सब चीजों से उठकर समता की ओर जो भी प्रयत्न हैं वे सब अच्छे हैं परन्तु इनसे त्रिगुणातीतता की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। गीता जिस समता की बात कर रही है वह एक बिल्कुल भिन्न चीज है। गीता में भगवान् अर्जुन को भिन्न-भिन्न प्रकार की समता समझाते हैं। श्रीअरविन्द उनका विस्तृत वर्णन करेंगे।
[गीता का] समत्व का जो पहला वर्णन है वह स्टोइक दार्शनिक के वर्णन के जैसा है। 'दुःखों के बीच जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों के बीच जिसे उनकी इच्छा नहीं होती, राग, भय, क्रोध से जो मुक्त हो चुका है वही स्थितधी मुनि है।' 'जो इस शरीर में काम-क्रोध से उत्पन्न होनेवाले वेग को सह सकता है वही योगी है, वही सुखी है।' तितिक्षा, अर्थात् सहने का अचवा बने रहने का संकल्प तथा शक्ति, इसका साधन है। 'शीत और ऊष्ण, सुख और दुःख देनेवाले जो भौतिक स्पर्श हैं, अनित्य हैं और आते-जाते रहते हैं, इन्हें सहना सीख। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये व्यथित नहीं करते न ही पीड़ा पहुँचाते हैं, जो दृढ़-स्थिर और बुद्धिमान् व्यक्ति सुख-दुःख में सम रहता है वह अपने-आप को अमरत्व के लिए उपयुक्त बना लेता है।' समत्वप्राप्त आत्मा को दुःख सहना होता है, पर वह दुःख से घृणा न करे, उसे सुख ग्रहण करना होता है, पर वह सुख से हर्षित न हो। शारीरिक यंत्रणाओं को भी सहनशीलता के द्वारा जीतना होता है और यह भी तपश्चर्यात्मक साधना के एक अंग के रूप में। जरा, मृत्यु, दुःख, यंत्रणा से बचकर भागना नहीं अपितु इन्हें स्वीकार कर के उच्च उदासीन स्थिति के द्वारा परास्त करना होता है। प्रकृति के निम्न-स्तरीय मुखौटों से भयभीत या स्तंभित होकर भागना नहीं, अपितु उसका सामना कर उसे विजित करना ही शक्तिशाली प्रकृति, पुरुषर्षभ, मनुष्यों के बीच किसी सिंह-समान आत्मा की सच्ची प्रवृत्ति है।
प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि उसे किसी सीमा तक सुख-दुःख आदि सहन करने का अभ्यास होना चाहिये। यदि व्यक्ति जरा से दुःख से प्रभावित होकर रोने लगता है और सुख में हर्षित हो जाता है तो वह मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है। यदि व्यक्ति को कोई महान् काम करना है तो सुख-दुःख में सम रहना तो परम् आवश्यक है। परन्तु लाखों में से कदाचित् कोई एक व्यक्ति भी ऐसा मिलना मुश्किल है जिसमें कि यह विशेष गुण हो पर जिसका अहं इसके कारण न फूलता हो, क्योंकि जब व्यक्ति सुख-दुःख आदि में अविचल रहता है, परास्त नहीं होता और सब परिस्थितियों में समान रहता है, उसके मन में अहं आए बिना नहीं रह सकता। इसलिए अकेले इस संयम से ही आगे का मार्ग नहीं खुलता, उसके लिए और भी चीजें आवश्यक हैं।
तापसी अथवा आत्मसंयमी (स्टोइक) ज्ञान वह है जो धैर्य के द्वारा जीव की आत्म-प्रभुत्व की शक्ति से प्राप्त होता है, एक ऐसी समता है जो अपनो प्रकृति से संघर्ष कर के प्राप्त की जाती है, और जिसे उसके स्वाभाविक विद्रोहों पर सतत् निगरानी रखकर और इनके विरुद्ध सतत् नियंत्रण रखकर बनाये रखा जाता हैः यह एक उत्कृष्ट शान्ति प्रदान करती है, एक तापसिक सुख प्रदान करती है, परन्तु यह उस मुक्त पुरुष का परम् आनन्द नहीं देती जो किसी नियम के अधीन नहीं, अपितु अपनी दिव्य सत्ता की विशुद्ध, सहज-स्वाभाविक पूर्णता में जीता है, जिससे कि वह 'चाहे जिस भी तरह कर्म करे तथा जीये, वह भगवान् में ही जीता और कर्म करता है', क्योंकि यहाँ पूर्णता केवल प्राप्त ही नहीं की जाती, अपितु स्वाधिकार से सदा अधिकृत भी रहती है तथा इसे बनाए रखने के लिए और प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह जीव का स्वभावमात्र बन चुकी होती है।
इस स्थिति में दोष यह है कि इसे बनाए रखने के लिए व्यक्ति को सतत् सजग और सतर्क रहना होता है। सदा ही व्यक्ति को उन ऊर्जाओं को, उस भाव को निरंतर बनाए रखना होता है जिनके सहारे वह निम्न प्रभावों से विचलित न हो सके। यह वह स्थिति नहीं होती जहाँ व्यक्ति निर्विघ्न रूप से, स्वच्छंद रूप से, सहज रूप से अपनी निम्न प्रकृति से ऊपर उठा होता है, और इसे बनाए रखने के लिए किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। यह वह स्थिति नहीं होती जिसे गीता कहती है कि 'जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर समस्त भूतों में मुझसे प्रेम करता है वह योगी चाहे जिस प्रकार रहे और कर्म करे मुझमें ही रहता और कर्म करता है।' गीता जिस स्थिति का वर्णन करती है उसमें व्यक्ति को प्रयत्न कर के अपने समत्व को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती। समत्व तो वहाँ सहज सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को किसी भी प्रकार के प्रयत्न या किसी दमन की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि निम्न चीजें व्यक्ति को विचलित कर ही नहीं सकतीं। यह स्थिति बहुत ही गहरी होती है जो प्राण और शरीर की सहनशीलता पर आश्रित नहीं होती। यह तो व्यक्ति की अंतरात्मा के भाव पर स्थित होती है।
गीता निम्न प्रकृति के साथ संघर्ष के अंदर हमारी सहनशीलता को और दृढ़ता अथवा धैर्य को प्रारंभिक साधन के रूप में स्वीकार करती है, परन्तु यदि अपनी व्यक्तिगत शक्ति के बल पर किसी प्रकार का प्रभुत्व प्राप्त होता है, तो भी इस प्रभुत्व की मुक्तावस्था केवल भगवान् से हमारे ऐक्य के द्वारा हो आती है, निजी व्यक्तित्व के एकमेव दिव्य पुरुष में लय या उनमें निवास द्वारा, तथा व्यक्तिगत इच्छा का भागवत् इच्छा में लोप हो जाने से ही प्राप्त होती है। ..... गीता की मुक्ति मुक्त पुरुष की मुक्ति है, वह निम्न प्रकृति से निकलकर परा प्रकृति में जन्म लेने से प्राप्त सच्ची मुक्ति है और वह अपनी दिव्यता में स्वतःस्थित रहती है। ऐसा मुक्त पुरुष जो कुछ भी करता है, चाहे जिस भी तरह जीता है, वह भगवान् में ही निवास करता है; वह घर का विशेष सुविधाप्राप्त या प्रिय बालक है, 'बालवत्' है जो कोई भूल नहीं कर सकता, जो कभी पतित नहीं हो सकता, क्योंकि वह जो कुछ भी है और जो कुछ भी करता है वह सब उस परम् पूर्ण, सर्वानन्दमय, सर्वप्रेममय और सर्वसौंदर्यमय से परिपूर्ण होता है।
जब व्यक्ति का परमात्मा के साथ ऐक्य होता है तब सहज रूप से वह सारी चीजों से ऊपर उठा होता है। इसके लिए उसे किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा को अपने भाव में बने रहने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। गीता के चौदहवें अध्याय में अर्जुन पूछता है कि नित्रैगुण्य के क्या लक्षण होते हैं। इसके प्रत्युत्तर में भगवान् कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने निम्न अंगों की वेदना तथा कामना, उनके हर्ष और शोक को मुस्कुराते हुए उनका अवलोकन करता है व उनसे विचलित नहीं होता, तथा प्रकाश और प्रसन्नता की स्थिति आने पर मोहित नहीं होता और केवल उच्चतर इच्छाशक्ति के निर्देशों की प्रतीक्षा करता है, वह निखैगुण्य होता है। वह ज्ञान-अज्ञान आदि से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। और यह स्थिति तभी प्राप्त की जा सकती है जब व्यक्ति ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। अन्त में भगवान् कहते हैं कि 'मेरी भक्ति के द्वारा यह स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि उस ब्रह्म का आधार भी मैं ही हूँ।' भगवान् की भक्ति के द्वारा सहज रूप से व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है। इस तरीके से गीता पुरुषोत्तम योग की ओर ले जाती है।
विशुद्ध दार्शनिक, मनीषी, जन्मजात-ज्ञानी पुरुष...सात्त्विक समता से आरंभ करता है। वह भी जड़भौतिक और बाह्य जगत् की क्षणभंगुरता को देखता है और कामनाओं को तुष्ट करने में या फिर सच्चा आनन्द प्रदान करने में इसकी असफलता को जानता है, परन्तु इससे उसे कोई शोक, भय या निराशा नहीं होती। वह सभी कुछ को स्थिर-शान्त विवेक बुद्धि से देखता है और बिना किसी विकर्षण अथवा घृणा या व्यग्रता के अपना चयन कर लेता है। 'इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होनेवाले ये भोग ही दुःख के कारण हैं, इनका एक आदि है और एक अंत है; इसलिए ज्ञानी, प्रबुद्ध बुद्धिवाला पुरुष (बुधः) इनमें रमण नहीं करता।' 'उसकी आत्मा इन बाह्य स्पशौं से अनासक्त रहती है; वह अपना सुख अपने ही अन्दर पाता है।...शत्रु, मित्र, तटस्थ और उदासीन सबके लिये वह आत्मभाव में सम होता है, क्योंकि वह देखता है कि ये सब अनित्य संबंध जीवन की परिवर्तनशील परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि विद्या, शुचिता, सदाचार के मिथ्याभिमान या बाह्याडंबर से तथा इन चीजों के आधार पर मनुष्य जो श्रेष्ठता के दावे आधारित करते हैं, इन सबसे वह भ्रमित या भ्रष्ट नहीं होता। वह साधु तथा असाधु के लिए, सदाचारयुक्त, विद्वान और सुसंस्कृत ब्राह्मण तथा पतित चांडाल के लिए, सभी मनुष्यों के लिए समभाव युक्त होता है। ये सभी गीता के सात्त्विक समता के वर्णन हैं, और ये पर्याप्त रूप से भली-भाँति उस सब को सार रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे संसार ज्ञानी मुनि की शांत बौद्धिक या दार्शनिक समता के रूप में जानता है।
समता के अतिरिक्त यहाँ अन्य कई महत्त्वपूर्ण विषय भी निहित हैं जिन पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। हमारे अंदर आनंद निहित है, परंतु वह सुषुप्त है और उस पर मन, प्राण, शरीर आदि का एक मोटा आवरण चढ़ा हुआ है। साथ ही हमारी प्राणिक सत्ता की जैसी संरचना है, वह जीवन के सभी अच्छे-बुरे, शुभ-अशुभ रूपों में आनन्द लेती है। जितना आनंद वह आराम, सुख तथा सफलता आदि में लेती है उतना ही आनंद उसे इनके विपरीत रूपों में भी मिलता है। और इसी कारण इस सृष्टि में ये सभी रूप हमें देखने को मिलते हैं। परंतु जैसा हमारा वर्तमान गठन है, हमें यह आनंद बड़े ही क्षीण रूप में तथा विकृत व परोक्ष रूप से इंद्रियों आदि के माध्यम से प्रास होता है। और जिन विशिष्ट प्रकार के स्पंदनों से यह आनंद हम तक पहुँचता है, उनके अभाव में हमारा उससे विछोह हो जाता है और हमें उस चीज का या व्यक्ति का विरह महसूस होने लगता है। चूंकि यह किसी के भी वश में नहीं है कि उसके पास केवल अनुकूल स्पंदन ही आएँ तथा प्रतिकूल न आएँ इसलिए यह आशंका सदा ही बनी रहती है कि कोई ऐसा स्पंदन न आ जाए जो सारे संतुलन को एकदम ही बिगाड़ दे। और इस कारण व्यक्ति सदा ही शंकित बना रहता है। ज्ञानी मनुष्य जब यह सब देखता है और इसका विश्लेषण करता है तब वह अनुभव करता है कि यह तो एक बड़ी ही दयनीय स्थिति है। वह अनुभव करता है कि सहज रूप से सच्चा आनंद तो उसके अपने अन्दर ही है, और यदि वह अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ जाए, जो कि आनन्दघन है, तब तो उसका आनन्द कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। परन्तु यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने इस सच्चे स्वरूप के अतिरिक्त अन्य दूसरे आकर्षणों की ओर ध्यान देना, उनके प्रति आकर्षित होना बंद कर दे और उनके प्रति उदासीन हो जाए। जब ये बाहरी चीजें व्यक्ति का ध्यान अतिशय रूप से आकर्षित करना और उसे अतिशय पीड़ा या फिर प्रसन्नता प्रदान करना बंद कर देती हैं तब व्यक्ति का ध्यान दूसरी ओर लग पाता है।
हमारे सामान्य स्तर से ऊपर के लोकों में श्रेष्ठता यह है कि वहाँ पीड़ा देने वाले स्पंदन जल्दी ही नहीं आ सकते इसलिए व्यक्ति को इनसे शंकित रहने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि हमारे सामान्य स्तर पर कोई भी स्पंदन आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूक्ष्म भौतिक स्तर पर एक निश्चित सीमा से नीचे की कोई चीज, कोई पीड़ा देने वाली चीज आ ही नहीं सकती। परंतु इसी तरीके से इसके ऊपर भी एक सीमा निर्धारित की गई है जिससे ऊपर का कोई स्पंदन उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। श्रीअरविन्द अपने सावित्री महाकाव्य में इस सूक्ष्म भौतिक जगत् का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार इस जगत् में वे सारी सुख-सुविधाएँ और सौंदर्य सहज ही उपलब्ध हैं जिनके लिये व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर दिन-रात मेहनत करता है और फिर भी उन्हें उपलब्ध नहीं कर पाता। यह सूक्ष्म भौतिक जगत् हमारे भौतिक जगत् के निकट ही है और हमारी आज की भौतिकवादी संस्कृति इसी से अपनी प्रेरणा लेती है। परन्तु जो सुख और सौंदर्य उस स्तर पर सहज ही उपलब्ध हैं वे यहाँ इस भौतिक जगत् में प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ अवचेतनता का दबाव बना रहता है। जबकि सूक्ष्म भौतिक जगत् में वह दबाव नहीं रहता।
उसके बाद में प्राणिक जगत् है। जहाँ सूक्ष्म भौतिक जगत् में उस जगत् विशेष की चीजों की ही प्रधानता होती है तथा प्राणिक चीजों का वहाँ अधिक प्रवेश नहीं होता और वहाँ केवल भौतिक सुख, सौंदर्य आदि ही प्रधान चीजें होती हैं, जबकि प्राणिक जगत् में प्राण ही प्रधान तत्त्व होता है और दूसरी सभी चीजें उसके अधीन होती हैं। भौतिक स्तर पर तो हमारे प्राणिक आवेगों, कामनाओं, इच्छाओं आदि पर शरीर की सीमितता तथा मन का अंकुश लगा होता है। परंतु प्राणिक जगत् में सभी कामनाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ, लोभ-लालच, दूसरों पर शासन करने की लालसाएँ आदि, तथा सभी भव्य और सुंदर चीजें जिनकी भौतिक जगत् में हम केवल कल्पना ही कर पाते हैं परंतु जो प्राप्त नहीं हो पातीं, वे सब सहज ही पूर्ण रूप से उपलब्ध होती हैं। परंतु वहाँ भी ऊपर मानसिक लोकों का और नीचे भौतिक लोकों का अंकुश तथा दबाव नहीं रहता। इन प्राणिक लोकों को स्वर्ग कहते हैं। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने प्राण को संतुष्ट करने के लिए जो भी इच्छा करता है, वह सब उस जगत् में हूबहू वैसा ही प्राप्त हो जाता है। वहाँ परिस्थितियाँ प्रतिकूल नहीं होतीं, व्यक्ति के संकल्प मात्र से ही सब कुछ संसिद्ध हो जाता है। इसीलिये उन्हें स्वर्ग कहते हैं। परन्तु यह सब कुछ आंतरिक नहीं अपितु केवल बाहरी ही होता है। इसके बाद में मानसिक जगत् आता है। इन सब सूक्ष्म भौतिक, प्राणिक और मानसिक जगतों में यह बाध्यता है कि वहाँ सब कुछ बाहरी स्पंदन पर निर्भर होता है। यद्यपि कोई भी गलत स्पंदन वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता परन्तु फिर भी अंततः व्यक्ति रहता तो बाहरी चीजों का ही दास है। अपने सच्चे स्वरूप में व्यक्ति जब स्वयं आनन्दघन है तब फिर किन्हीं बाहरी चीजों से संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना कोई अधिक संतोषजनक स्थिति नहीं है जिसमें व्यक्ति बाहरी माध्यमों के द्वारा, मन, प्राण, शरीर और इन्द्रियों के द्वारा सुख बटोरने का प्रयास करता है। परन्तु आत्मा का आनन्द सहज है जिसे किन्हीं माध्यमों की आवश्यकता नहीं है और वह असीम है। इसीलिये हमारे ऋषि-मुनि इन सूक्ष्म भौतिक, प्राणिक और मानसिक स्वर्गों से अधिक अभीभूत नहीं होते थे क्योंकि वे जानते थे कि भले ही अपने-आप में ये स्वर्ग कितने भी समृद्ध और वैभवशाली क्यों न हों, तो भी आंतरात्मिक आनंद और वैभव से इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती।
अब यहाँ सात्त्विक समता की बात करते हुए श्रीअरविन्द कहते हैं कि सात्त्विक व्यक्ति को संसार की क्षणभंगुरता और अनित्यता का बोध होता है और वह जान जाता है कि सांसारिक चीजों से विचलित होना या उनमें संतुष्टि पाने का प्रयत्न करना निरर्थक है। वह इन सब चीजों में अपनी चेतना को नहीं फँसाता और इनसे प्रभावित न होकर मित्र-शत्रु, प्रिय-अप्रिय, सफलता-विफलता आदि सभी को समान दृष्टि से देखकर सबसे समान व्यवहार करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर कर के उसके द्वारा अपनी इन्द्रियों और अपने सारे क्रिया-कलाप पर यथासंभव अधिक-से-अधिक प्रभाव डालता है - हालाँकि बुद्धि के माध्यम से एक सीमा से अधिक प्रभाव तो वह नहीं डाल सकता और वह उस सात्त्विक अथवा दार्शनिक की समता की ओर बढ़ता है जिसके बारे में श्रीअरविन्द बता रहे हैं।
प्रश्न : क्या ज्ञानी या दार्शनिक की समता निषेधात्मक होती है चूंकि उसे सभी चीजें निःसार प्रतीत होती हैं?
उत्तर : जब व्यक्ति को किसी गहरी चीज में रस आने लगता है और उसकी बुद्धि को बाहरी चीजों में कोई रस नहीं रह जाता तब फिर ये चीजें उसकी नजर में कोई महत्त्व ही नहीं रखतीं। इसीलिए इन बाहरी चीजों में बदलाव आने पर या फिर कोई उतार-चढ़ाव आने पर भी वह इनसे विचलित नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि शेयर बाजार में आपकी कोई रुचि ही नहीं है और न ही आपका उसमें कोई पूँजी निवेश है तो उसमें आए उतार-चढ़ाव से आप क्यों प्रभावित होने लगे? इसी प्रकार ज्ञानी या दार्शनिक की बुद्धि को इन बाहरी चीजों में कोई रस नहीं रह जाता। यह बात याद रखने की है कि केवल बुद्धि ही यह भाव अपनाती है और आवश्यक नहीं है कि उसके अन्य भाग भी इसमें सम्मिलित हों और उनमें भी समता का भाव हो। हो सकता है कि शरीर में समता न हो, या फिर प्राण में समता न हो। या फिर हो सकता है कि बुद्धि के साथ-ही-साथ हृदय, आत्मा या सत्ता के अन्य भाग इसमें सम्मिलित हों। परन्तु आवश्यक नहीं है कि सभी भागों में समता स्थापित हो जाए क्योंकि सभी भागों में व्यक्ति के अवचेतन तथा जड़-भौतिक भागों का प्रवेश और उनका प्रभाव रहता है जो कि ऐसी समता को स्वीकार नहीं करते। विशेषकर प्राण में और जड़-भौतिक भागों में समता स्थापित होना तो बहुत ही मुश्किल है। परन्तु बुद्धि और हृदय की समता का स्थापित होना भी व्यक्ति के जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव डालता है जिसे देखकर सामान्य लोग उसे बहुत ही महान् व्यक्तित्व के रूप में देखने लगते हैं, क्योंकि जिन बाहरी चीजों में सामान्य जन बहुत अधिक आसक्त रहते हैं और अत्यधिक प्रयास के बाद भी जिन चीजों से ऊपर नहीं उठ पाते उनसे तो वह आकर्षित ही नहीं होता और उनके नष्ट हो जाने पर विचलित नहीं होता। परंतु जिसमें ऐसी समता स्थापित हो गई है वह इसलिये होती है क्योंकि वह इन बाहरी चीजों की क्षणभंगुरता को जान चुका होता है और इसलिए उसमें समता स्थापित होना तो स्वाभाविक ही है।
प्रश्न : तो इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति का विवेक जागृत हो गया है?
उत्तर : हाँ, क्योंकि बुद्धि के प्रभाव से ही तो वह जागृत हो जाता है। बुद्धि सत्त्व-गुण प्रधान है, प्राण रजस् प्रधान है और भौतिक तमस् प्रधान है। इसलिए जब बुद्धि को बाहरी चीजों की अनित्यता का बोध प्राप्त हो जाता है तब उसमें समता आ जाती है। परंतु एक विचार के रूप में ही यह जान लेना कि केवल भगवान् ही अच्छे हैं और सब कुछ बेकार है, अधिक प्रभावशाली नहीं होता। परंतु जब अंतर से यह भाव आता है और अन्तरात्मा प्रबल होती है और वह बुद्धि के द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करती है तभी वह हमें ऊपर उठा पाती है। केवल एक विचार मात्र से यह कभी नहीं हो सकता। विचार रूप से तो अधिकांश लोग ये सब बातें जानते ही हैं। हमारे सारे शास्त्र ऐसी सब शिक्षा से भरे पड़े हैं कि संसार अनित्य है, इसमें मोह नहीं रखना चाहिये। साथ ही यह कहा जाता है कि यह सब मोह-माया जीवन नष्ट होने पर व्यक्ति के साथ नहीं जाती और सब कुछ यहीं रह जाता है। परंतु जिसके अंदर आत्मा के प्रभाव से बुद्धि में यह समता आ गई है उसे तो यह बात बड़ी ही सुखद प्रतीत होती है कि कम-से-कम ये सब अनित्य चीजें साथ नहीं जाएँगी, अन्यथा तो जीवन के अंत के बाद भी ये ही चीजें पीछा करती रहेंगी तो यह तो बड़ा ही भयंकर होगा। इस प्रकार बुद्धि में यह समता स्थापित होने पर संपूर्ण दृष्टिकोण ही बदल जाता है।
गीता बार-बार कहती है कि जो अवलोकन करता है, उसे पुरुष कहते हैं और जिसका अवलोकन किया जाता है, वह प्रकृति है। अवलोकन करने की यह क्षमता ही मनुष्यों को पशुओं से भिन्न करती है। परंतु साक्षित्व करने का स्तर प्रत्येक मनुष्य की चेतना के अनुसार भिन्न-भिन्त्र होता है। व्यक्ति अपनी सतही चेतना से कुछ अलग हटकर साक्षित्व कर सकता है, कुछ उससे अधिक गहरी अवस्था से साक्षित्व कर सकता है, और जो बहुत अधिक विकसित होता है वह अपने चैत्य या अंतरात्मा से चीजों का अवलोकन कर सकता है। परंतु सामान्यतया मनुष्य जिस सतही चेतना में रहते हैं उसमें उनका साक्षित्व भी बहुत ही सतही होता है इसीलिए जीवन भर ठोकरें खाते हुए भी वे उन्हीं भूलों को दोहराते रहते हैं और उन्हीं चीजों में लिप्त रहते हैं। व्यक्ति का साक्षित्व का स्तर जितना ही गहरा होगा उतना ही वह शक्तिशाली होगा क्योंकि उतना ही अधिक वह परमात्म तत्त्व के निकट होगा और उतनी ही अधिक उसमें जीवन पर प्रभाव डालने की तथा उसे परिवर्तित करने की शक्ति होगी। इसलिए महत्त्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति साक्षित्व कहाँ से और किस गहराई से करता है उसी पर यह समता निर्भर करती है। इसे सात्त्विक या दार्शनिक समता कहते हैं। गीता में इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं जैसे कि 'जो ज्ञानी है वह न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करता है'।
ii. 11
प्रश्न : क्या ऐसा नहीं है कि इस सात्त्विक समता से पहले जो तापसी (स्टोइक) प्रकार की समता के बारे में बताया गया है वह तो पुरुषार्थ से प्राप्त की जाने वाली समता है, परन्तु यह ज्ञान की जो समता है इसके पाने के लिये तो अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती?
उत्तर : चूंकि यह सात्त्विक प्रकार की समता है इसलिए इसमें श्रम अपेक्षाकृत कम लगता है। जैसे कि यदि हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं तो हमारे अन्दर जितनी ही अधिक शक्ति होगी उतनी ही कम मेहनत उसे जीतने में हमें करनी होगी और जितनी कम शक्ति होगी उतनी ही अधिक मेहनत करनी होगी। वैसे ही सात्त्विक समता में शक्ति अधिक होती है इसलिए इसका प्रभाव अधिक होता है और सहज रूप से ही अन्य भागों पर इसकी क्रिया होती है। इस समता में आत्मा बुद्धि के द्वारा अपना प्रभाव डालती है। तापसी समता में आत्मा भौतिक चेतना के द्वारा, संवेदनों के द्वारा काम करती है। अलग-अलग व्यक्तियों का अलग-अलग संतुलन होता है। यह तो भगवान् की विचित्र लीला है। फिर भी, व्यक्ति समता तभी रख सकता है जब अन्दर की कोई गहरी चीज उसे प्रश्रय दे। अन्यथा अधिकांश व्यक्ति तो अपनी इन्द्रियों के ही गुलाम बने रहते हैं क्योंकि बिना किसी आंतरिक आधार के इन्द्रियों से ऊपर उठना संभव नहीं है। बहुत से लोग ज्ञान का प्रदर्शन तो बहुत करते हैं परन्तु जरा-सी बीमारी से भी विचलित हो उठते हैं क्योंकि उनमें सहन करने की शक्ति नहीं होती। इसके विपरीत कई व्यक्तियों को कोई समझ तो नहीं होती परन्तु फिर भी वे अन्दर से बहुत मजबूत होते हैं और किसी भी चीज की परवाह ही नहीं करते। हालाँकि इसका यह अर्थ नहीं है कि इस कारण से ये बहुत महान् व्यक्ति हो गये और दूसरे बड़े ही हीन हो गये। इनमें बस अंतर इतना ही है कि एक की भौतिक चेतना में किसी गहरी चीज का सहारा है जबकि दूसरे को वह सहारा भौतिक चेतना में न प्राप्त होकर बुद्धि में प्राप्त है। हाँ, यदि बुद्धि के साथ हृदय, प्राण, भौतिक आदि सभी चीजों में यह समर्थन प्राप्त हो तो बहुत ही अच्छा है। गीता इन समताओं के बारे में बात तो करती है परन्तु वास्तव में जिस समता को वह चाह करती है वह तो परम् स्थिति है जो कि व्यक्ति की सम्पूर्ण सत्ता को ही परिवर्तित कर देती है और यह समता भगवान् के साथ ऐक्य से आती है जो कि अनंत है। यह समता आने पर संपूर्ण ब्रह्माण्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो व्यक्ति को विचलित कर सके क्योंकि यदि परमात्मा ही ब्रह्माण्ड की चीजों से विचलित होते तब फिर वह इन चीजों के दास हुए, न कि इनके स्वामी। अतः गीता की समता भगवान् के साथ एकत्व से आने वाली समता है। अन्य सभी तरीके तो उस एकत्व को प्राप्त करने के और उस समता तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं। किसी-किसी के लिए यह भी संभव हो सकता है कि वह बिना किसी विशिष्ट मार्ग का अनुसरण किए सीधे ही परमात्मा तक पहुँच जाए। क्योंकि सबके लिये कोई एक ही तय नियम लागू नहीं होता। भगवान् के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता। उनके विधान में जैसा उन्हें उचित लगता है वे वैसा ही करते हैं। अतः सब कुछ व्यक्ति-व्यक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है।
तो यहाँ हमने तामसिक और सात्त्विक दो प्रकार की समता के विषय में चर्चा की है।
यह दार्शनिक उदासीनता की समता है; यह एक उच्च शांत-स्थिरता तो लाती है परंतु महानतर आध्यात्मिक हर्ष नहीं लाती; यह तो एक एकाकी या अलग-थलग मुक्तावस्था है... जो अंततः संसार से अलग-थलग और निष्प्रभावी है। दार्शनिक मनोभाव की उदासीनता को गीता एक प्रारम्भिक प्रवृत्ति के तौर पर स्वीकार करती है; परन्तु जिस उदासीनावस्था तक गीता अंततः लाती है - उसके लिए यदि इस अपर्याप्त शब्द 'अलगाव' का किसी तरह से व्यवहार किया भी जाए तो - उसमें दार्शनिक अलगाव का भाव नहीं है। निःसंदेह वह 'उदासीनवत्' उच्चासीन होना है अवश्य, पर वैसे ही जैसे भगवान् ऊर्ध्व में आसीन हैं, जिन्हें इस जगत् में किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे सतत् कर्म करते हैं और सर्वत्र ही प्राणियों के उद्यम या पुरुषार्थ को आश्रय प्रदान करते हुए, सहायता प्रदान करते हुए और उनका मार्गदर्शन करते हुए विद्यमान रहते हैं। यह समता सब प्राणियों के साथ एकत्व पर प्रतिष्ठित है। इसमें उस चीज का भी समावेश होता है जिसका दार्शनिक समता में अभाव होता है; क्योंकि इसकी आत्मा शान्ति की आत्मा है और साथ ही वह प्रेम को आत्मा भी है। यह अशेष रूप से सभी जीवों को भगवान् के अंदर देखती है. यह व्यक्तिगत आत्मा का सर्वभूतात्मा के साथ एक हो जाना है और इसलिए यह सभी भूतों के साथ परम् सहानुभूति या तालमेल में रहती है। इस सर्वव्यापी, सर्वभावेन सहानुभूति और आध्यात्मिक का एकत्व न केवल उस सब के साथ है जो शुभ हो, सुन्दर हो और रुचिकर हो, अपितु, ऐसी किसी चीज को या किसी भी व्यक्ति को अशेषेण, निरपवाद रूप से, इससे अलग नहीं रखा जा सकता भले वह दिखने में कितना भी नीच, पतित, पापी या घृणित क्यों न हो। यहाँ न केवल मात्र घृणा अथवा क्रोध अथवा अनुदारता के लिए ही कोई स्थान नहीं है, अपितु अलगाव, अवहेलना या अपनी श्रेष्ठता के किसी प्रकार के क्षुद्र गर्व के लिए भी यहाँ कोई स्थान नहीं है। किसी बाह्य इंद्रियाश्रित व्यक्ति के लिए इस समता में संघर्षरत मन की अज्ञानता के प्रति एक दिव्य करुणा प्रतीत होगी, उस पर समस्त प्रकाश और शक्ति और सुख की वर्षा करने के लिए एक दिव्य संकल्प अवश्य प्रतीत होगा; परंतु उसके अन्दर की दिव्य आत्मा के प्रति उसमें इनसे भी कोई बड़ी चीज होगी, उसके प्रति होंगे चाह और प्रेम। क्योंकि सबके भीतर से, जैसे साधु महात्मा के अन्दर से वैसे ही चोर, वेश्या और चाण्डाल के अन्दर से भी वे ही प्रियतम झाँकते हैं और पुकार कर कहते हैं, 'यह मैं हूँ।' 'जो सब भूतों में मुझसे प्रेम करता है वह योगी चाहे जिस प्रकार रहे या कर्म करे, मुझमें ही रहता और कर्म करता है' - दिव्य सर्वव्यापी प्रेम की परम् प्रगाढ़ताओं और गंभीरताओं के लिए इससे अधिक शक्तिशाली वाणी का प्रयोग संसार के और किस दर्शनशास्त्र या धर्म में हुआ है?
vi.31
दार्शनिक या सात्त्विक समता के आने पर भी व्यक्ति में तत्त्वतः कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता और वह जैसा मूलतः था लगभग वैसा हो क्यों बना रहता है, इसका कारण यहाँ बताया गया है। वह यह है कि सात्त्विक समता और आत्मा की समता में सारा ही अन्तर है, जिसे समझना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आत्मा की समता का आधार पूर्ण एकत्व में है न कि जगत् की निःसारता या उसकी क्षणभंगुरता के बोध से उत्पन्न होने वाले समत्व के भाव में। आत्मा की समता में व्यक्ति स्वयं को सम्पूर्ण जगत् के साथ एकमय महसूस करता है। सात्त्विक समता वाला व्यक्ति इस संसार के नाटक से अपने-आप को अलग करने का और इससे ऊपर उठने का भाव रखता है जबकि आत्मा की समता में व्यक्ति स्वयं एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए भी अपने-आप को सभी घटनाओं और पात्रों के साथ एकमय महसूस करता है फिर चाहे वे पात्र नायक हों या खलनायक। मानो वह स्वयं ही सबमें विद्यमान हो। उसे यह महसूस होता है कि यह सब उसका अपना ही खेल चल रहा है और उसमें वह अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है और आनन्द ले रहा है।
आत्मा की समता उदासीनवद् या अलगाव की समता नहीं है, जिसमें व्यक्ति को किसी चीज से कोई मतलब ही न हो। यह समता तो पुरुषोत्तम की समता है। जैसा कि भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके पास न हो, फिर भी वे सदा कर्म में रत रहते हैं और कदम-कदम पर इस संसार और प्राणियों की सहायता करते हैं। क्योंकि यहाँ उदासीन होकर निर्लिप्त रहने की बात नहीं होती अपितु प्रेम का संबंध होता है। इस भाव में व्यक्ति सभी के अंदर स्वयं अपने-आप को ही देखता है इसलिए वह विचलित नहीं होता क्योंकि वह स्वयं ही सब जगह मौजूद है और यह सारा खेल उसी का चल रहा है। जब हम किसी नाटक के स्वयं ही निर्देशक और प्रतिभागी हैं तो उस नाटक के अच्छे-बुरे दृश्यों को देखकर विचलित नहीं होने वाले। और चूँकि इसमें सभी पात्रों के साथ व्यक्ति एकत्व महसूस करता है इसलिये वह पात्रों के साथ कोई ऊपरी समता नहीं रखता वरन् उसमें आनंद लेता है और उस नाटक में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हुए दूसरों को भी अपनी-अपनी भूमिका बखूबी निभाने में सहायता करता है, भले वे पात्र नायक हों या खलनायक।
और जब व्यक्ति सबके अन्दर स्वयं को देखता है, अपने प्रियतम को देखता है, परमात्मा को देखता है तो इससे बड़ा आनन्द तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे भाव में फिर जरा-से भी कष्ट का या किसी प्रकार के उत्पीड़न के अनुभव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अन्य सभी प्रकार की समता में हमें शान्ति तो प्राप्त हो सकती है परन्तु वह कोई आनन्द नहीं देने वाली, जबकि आत्मा की समता आनन्ददायी है। श्रीअरविन्द ने गीता के इस श्लोक का वर्णन करते हुए कहा है कि इससे बड़ी बात तो कभी किसी ने कही ही नहीं है जिसमें भगवान् कहते हैं कि जो सब भूतों में मुझसे प्रेम करता है वह योगी चाहे जिस प्रकार भी रहे या कर्म करे, मुझमें ही रहता और कर्म करता है। जब व्यक्ति ऐसी चेतना में निवास करता है और यह जान लेता है कि परमात्मा में ही सब कुछ है और वह सभी जीवों में परमात्मा को ही देखता है, उसके आनन्द का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह स्थिति परम् आनन्द की स्थिति है। ऐसे व्यक्ति के लिए समता-असमता तो खेल मात्र रह जाते हैं। गीता इसी समता की ओर ले जा रही है जिसमें व्यक्ति परमात्मा से एक हो जाता है। यहाँ सात्त्विक समता और आत्मा की समता के बीच तुलना कर के दर्शाया गया है कि किस प्रकार से सात्त्विक समता अपने-आप में अपर्याप्त है।
प्रश्न : इसमें उदासीनवद् शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है?
उत्तर : उदासीनवद् का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। उदासीनवद् अर्थात् व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर है। जैसे आप किसी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं तो आप उसमें भागीदार तो पूरे हैं परन्तु आपके लिए सभी दृश्य समान हैं और आप उनको देखकर विचलित नहीं होते क्योंकि आप स्वयं ही भूमिका निभाने वाले, स्वयं ही निर्देशन करने वाले और स्वयं ही दर्शक भी होते हैं। मानसिक चेतना में तो व्यक्ति इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकता और उसे इन सबका बोध भी नहीं होता।
ईश्वरेच्छाधीनता - भगवदेच्छा के अधीन हो जाना, धैर्य के साथ सूली (दुःख-कष्टों) को सहन करना, विनीत भाव से सहिष्णु होना - एक प्रकार की धार्मिक समता का आधार है। यह भगवदेच्छा की अधीनता का तत्त्व गीता में एक अधिक विशाल रूप धारण कर लेता है और समग्र सत्ता का भगवान् के प्रति पूर्ण समर्पण बन जाता है। यह केवल निष्क्रिय अधीनता नहीं है, अपितु एक सक्रिय आत्म-दान है; यह समस्त वस्तुओं में भगवान् की इच्छा को देखना और स्वीकार करना भर नहीं है, अपितु अपनी निजी इच्छा को कर्मों के प्रभु को उनका उपकरण बनने के लिए सौंप देना है, और वह भी भगवान् का एक सेवक बनने के लघुतर भाव से नहीं, अपितु अंत में कम-से-कम इस भाव से कि वह अपनी चेतना और अपने कर्म, दोनों का ही उनमें संपूर्ण संन्यास कर दे, ताकि उसकी सत्ता भगवान् की सत्ता के साथ एक हो जाए और उसकी नैयक्तिक प्रकृति यंत्रमात्र रह जाए, और कुछ नहीं। हर फल या परिणाम को चाहे अच्छा हो या बुरा, प्रिय हो या अप्रिय, शुभ हो या अशुभ, उसे कर्मों के प्रभु भगवान् का मानकर स्वीकार किया जाता है, जिससे कि अंततः शोक और दुःख को केवल सहन ही नहीं किया जाता, अपितु उन्हें निष्कासित कर दिया जाता हैः भावात्मक मन (चित्त) की पूर्ण समता प्रतिष्ठित हो जाती है। उपकरण में तब वैयक्तिक इच्छा या संकल्प का भान नहीं होता; यह दिखाई देता है कि सभी कुछ पहले से ही विराट् पुरुष के सर्वज्ञ पूर्वज्ञान और उनकी सर्वसमर्थ अमोघ शक्ति में पहले ही संपन्न हो चुका है और मनुष्यों का अहंकार उस भागवत् संकल्प की क्रियावली को नहीं बदल सकता। इसलिए अंतिम मनोभाव वह होगा जिसका निर्देश अर्जुन को आगे के अध्याय में बताया गया है, 'सब कुछ मेरे द्वारा मेरी दिव्य इच्छा और पूर्वज्ञान में पहले ही किया जा चुका है; हे अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन', निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। यह मनोभाव निश्चय ही अंततः वैयक्तिक इच्छा के भागवत् संकल्प के साथ पूर्ण ऐक्य तक ले जाएगा और, ज्ञान की वृद्धि के साथ ही जीव रूपी उपकरण की भागवत् शक्ति और ज्ञान के अनुकूल दोषरहित अनुक्रिया या प्रत्युत्तर ले आएगा। परात्पर, विराट् और व्यष्टि पुरुष के इस परम् ऐक्य की संतुलित अवस्था में आत्म-समर्पण की पूर्ण और निरपेक्ष समता होगी, मन होगा दिव्य ज्योति और शक्ति की निष्प्रतिरोध वाहिका और सक्रिय सत्ता बन जाएगी जगत् में इस दिव्य ज्योति और शक्ति के कार्य के लिए एक पराक्रमी अमोघ यंत्र।
जैसा कि श्रीअरविन्द ने पहले तापसी समता और दार्शनिक या सात्त्विक समता के बारे में वर्णन करते हुए उनका स्वरूप और उनकी सीमा और अपर्याप्तता दर्शायी थी और गीता में वर्णित समता से उसकी तुलना की थी, उसी प्रकार यहाँ वे धार्मिक समता का वर्णन कर रहे हैं। तीसरे प्रकार की यह समता हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लोग इससे आरम्भ करते हैं। हिन्दुस्तान में अधिकतर लोग आस्तिक हैं, इसलिये यहाँ मनोवैज्ञानिक समस्याएँ पश्चिम की तुलना में बहुत कम हैं। पश्चिम के विपरीत यहाँ भारत में यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई धोखा हो जाता है या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है जिससे उसे आघात पहुँचता है तो उसे पीड़ा तो होती है परंतु इसके साथ-ही-साथ कहीं न कहीं उसमें यह भाव भी उठता है कि भगवान् जो कुछ भी करते हैं उसके भले के लिए ही करते हैं। यह एक सर्वसामान्य सुझाव है जिससे बहुत-सी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को अधिक बल नहीं मिल पाता और धीरे-धीरे उनका स्वतः ही अंत हो जाता है और व्यक्ति को जिस अतिशय पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ सकता था उससे उसे बहुत कुछ राहत मिल जाती है। यहाँ भारत में हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि व्यक्ति किसी-न-किसी आध्यात्मिक गुरु से, किसी मंदिर, देवता, इष्ट आदि से संबद्ध होता है, उसमें आस्था रखता है। और जिसमें उसे आस्था होती है उसे वह अपनी तकलीफें, अपनी समस्याएँ बताता है और एक बड़ी भारी मनोवैज्ञानिक राहत महसूस करता है। उदाहरण के लिए अपने किसी स्वजन की या अपने किसी घनिष्ठ संबंधी या मित्र की मृत्यु पर व्यक्ति को बहुत ही गहरी पीड़ा होती है। परंतु यहाँ यह विचार प्रचलित है कि सब कुछ भगवान् को मर्जी से होता है और वे सदा भला ही करते हैं चाहे बाहर से हमें वह चीज कितनी भी अप्रिय या दुःखद क्यों न प्रतीत हो रही हो, इसलिए ऐसा उनका विधान मानकर वह कम-से-कम अपनी बुद्धि में तो उस पीड़ा से कुछ राहत पाता है। यदि यह धार्मिक भाव न होता तो जिस भयंकर मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक पीड़ा से व्यक्ति को गुजरना पड़ता उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए पश्चिम की संस्कृति में ऐसे किसी सहारे के अभाव में हम बहुत से लोगों को अपना मानसिक संतुलन तक खोते देखते हैं।
परंतु इस स्तर से आगे बढ़ने पर व्यक्ति सोचता है कि जब बिना परमात्मा की इच्छा के कुछ नहीं होता, और जो होता है वह अच्छे से अच्छा ही होता है तब उसे किसी चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी उसके साथ होता है, वह चाहे सुखदायी हो या दुःखदायी, उसके लिए वह तो भगवान् को निर्विवाद रूप से धन्यवाद हो देगा। इसलिए वह किन्हीं भी परिस्थितियों में अधिक विचलित नहीं होता। हो सकता है कि किसी घटना से वह कुछ समय के लिए विचलित हो, परंतु इस मनोभाव के कारण शीघ्र ही वह उसमें से बाहर निकल आता है। इस समता का स्थान व्यक्ति के हृदय में होता है, और वह भगवान् को समर्पित होता है। व्यक्ति यह सोचता है कि उसके प्रभु ही सारे संसार को चला रहे हैं इसलिए जो कुछ भी होगा वह तो अच्छा ही होगा। ये सभी प्रकार की समताएँ गीता में हैं, परन्तु गीता यहीं नहीं रुक जाती। हमारी संस्कृति में पहले स्तर की धार्मिक समता तो साधारणतया सभी में पायी जाती है। उससे आगे फिर कुछ लोग और अधिक गहराई में चले जाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह भगवान् की इच्छा से ही होता है। इससे और आगे का मनोभाव यह है कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं व्यक्ति उसे केवल स्वीकार ही नहीं करता और उसके प्रति अपनी सहमति ही व्यक्त नहीं करता, अपितु अपने गुरु की या भगवान् की इच्छा जानकर वह उसमें आनन्द लेने लगता है। इसलिये गीता कहती है कि जब व्यक्ति के अन्दर यह भाव अधिक गहरा होता जाता है तो वह अपनी बाहरी यांत्रिक प्रकृति से ऊपर उठकर प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की हो इच्छा देखकर उसमें गहरा आनन्द लेना आरम्भ कर देता है। उसे उसमें इतना आनन्द आने लगता है कि उसके लिए किन्हीं भी बाहरी चीजों का, बाहरी घटनाओं का - चाहे वे कितनी भी प्रिय-अप्रिय, सुखद या दुःखद क्यों न हो – कोई मूल्य नहीं रह जाता। और जब व्यक्ति को इतना अधिक आनन्द आने लगता है तो वह भगवान् को समर्पित एक ऐसा निष्ठावान् यंत्र बन जाता है कि भगवद्-इच्छा के लिये वह कुछ भी करने को तैयार रहता है क्योंकि उसे सर्वत्र प्रभु की इच्छा ही दिखाई देती है। इसीलिये भगवान् अर्जुन को कहते हैं कि तू तो केवल निमित्त मात्र बन। इस भाव में व्यक्ति जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभु के द्वारा किया जा रहा है, उसे तो निमित्त मात्र बनना है। और जब सारी शक्ति, ऊर्जा, धीरज, प्रेम आदि सब कुछ स्वयं प्रभु ही उसे प्रदान कर रहे हैं तब उसे तो केवल निमित्त बनकर किसी भी कर्म को संपादित करने में समस्या ही क्या हो सकती है। तब व्यक्ति चेतना की उस पराकाष्ठा तक पहुँच जाता है जहाँ वह परमात्मा के साथ ऐक्य की ओर अग्रसर होता है और आत्मा की समता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार एक सतही धार्मिक भाव से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए वह इस आत्मा की समता तक आ सकता है और परमात्मा के साथ पूर्ण ऐक्य तक आ सकता है।
कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति चाहे कहीं से भी आरंभ करे, चाहे तापसी समता या दार्शनिक समता से आरंभ करे या फिर धार्मिक समता से, परन्तु गीता व्यक्ति को परमात्मा से ऐक्य की समता की ओर ले जाती है। हालाँकि उस स्थिति को समता का नाम ही नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह तो दिव्य स्थिति है। सारांश यह है कि व्यक्ति चाहे कहीं से भी आरम्भ क्यों न करे उसे किसी भी अवस्था विशेष पर रुकना नहीं चाहिए और यदि वह उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो अन्त में भगवान् के साथ अधिकाधिक ऐक्य साधता जाता है। गीता अपनी सारी साधना इसी क्रम से विकसित करती है और फिर अंत में :
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।। १८.६५।।
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। १८.६६।।
इस स्थिति की ओर बढ़ना ही तो संपूर्ण जीवन का सार है। भले ही हमने कितनी भी ऊँची स्थिति क्यों न प्राप्त कर ली हो, परंतु कहीं भी रुकना नहीं है। क्योंकि हमारे सामने अनंत भवितव्यताएँ हैं। और गीता भी हमें कहीं बीच की अवस्था में रोके बिना सीधे अतिमानस के छोर तक ले जाती है।
इस अवस्था में हमारे ऊपर दूसरों की क्रिया (व्यवहार) के प्रति भी समता रहेगी। वे ऐसा कोई व्यवहार या क्रिया नहीं कर सकते जो उस आंतरिक एकत्व, प्रेम और सहानुभूति (सामंजस्य) में कोई अन्तर डाले, जो कि सभी में एक ही आत्मा के, सभी प्राणियों में व्याप्त भगवान् के प्रत्यक्ष बोध से उत्पन्न होती है। परन्तु व्यवहार में ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसमें दूसरे लोगों और उनकी क्रियाओं के प्रति निष्प्रतिरोध सहिष्णुता तथा अधीनता का, सहनशील निर्विरोध स्वीकृति का भाव हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान् और वैश्व संकल्प का उपकरण होकर सतत् आज्ञाकारिता का अवश्य ही यही तो अभिप्राय है कि जगत् में विरोधी शक्तियों का जो संघर्ष चल रहा है उसमें उन वैयक्तिक कामनाओं से युद्ध करना जो निश्चय ही अपनी निजी अहंमय तुष्टि चाहती हैं। इसीलिए अर्जुन को आदेश दिया गया है कि वह प्रतिरोध करे, युद्ध करे और विजय प्राप्त करे; परंतु द्वेष-रहित होकर अथवा व्यक्तिगत कामना या व्यक्तिगत शत्रुता या वैर-भाव छोड़कर लड़े, क्योंकि मुक्त पुरुष के लिए ये भाव असंभव हैं। लोगों को भगवन्मार्ग पर बनाए रखने और चलाने के लिए, निरहंकार रूप से, लोकसंग्रह के लिए कर्म करना, वह धर्म या विधान है जो भगवान् के साथ, विश्व-पुरुष के साथ अपनी अंतरात्मा की एकता से स्वभावतः उत्पन्न होता है, क्योंकि विश्व के अखिल कर्म का संपूर्ण अभिप्राय और लक्ष्य यही है। सभी जीवों के साथ हमारी एकता से इस कर्म का कोई विरोध नहीं है, यहाँ तक कि उनसे भी कोई विरोध नहीं है जो यहाँ विरोधियों और शत्रुओं के रूप में प्रस्तुत हैं। क्योंकि भगवान् का जो लक्ष्य है वही उनका भी लक्ष्य है, क्योंकि वही सबका अप्रत्यक्ष लक्ष्य है, यहाँ तक कि उन जीवों का भी जिनके बहिर्मुख मन अज्ञान और अहंकार से विभ्रमित होकर पथ से भटका करते हैं और अपनी अंतःप्रेरणा का प्रतिरोध किया करते हैं। उनका प्रतिरोध करना और उन्हें पराजित करना ही उनकी सबसे बड़ी बाह्य सेवा है। इस दृष्टि के द्वारा गीता उस अपूर्ण सिद्धांत से बच जाती है जो समता की एक ऐसी शिक्षा से उत्पन्न हो सकता था जो अव्यावहारिक रूप से समस्त संबंधों की अवहेलना करती हो और जो उस दुर्बलकारी प्रेम की शिक्षा से उत्पन्न हो सकता था जिसके मूल में ज्ञान का सर्वथा अभाव होता है, जबकि गीता उस सारभूत तत्त्व को अक्षुण्ण बनाए रखती है। अंतरात्मा के लिए सबके साथ एकत्व, हृदय के लिए अचल विश्व-प्रेम, सहानुभूति और करुणा; परन्तु हाथों के लिए नैर्व्यक्तिक रूप से हित-साधन करने का स्वातंत्र्य - ऐसा हित-साधन नहीं जो भगवान् की योजना का कोई विचार न करे या उसके विरुद्ध जाकर इस या उस व्यक्ति के सुख-साधन में लग जाए, अपितु ऐसा हित-साधन जो सृष्टि के हेतु का सहायक हो, जिससे मनुष्यों को अधिकाधिक सुख और श्रेय प्राप्त हो, सब भूतों का संपूर्ण कल्याण हो।
गीता की इन सब बातों का अधिकांश लोग बिल्कुल गलत अर्थ लगाते हैं कि सबसे प्रेम करो, किसी से भी राग-द्वेष मत करो, सबके साथ समान व्यवहार करो आदि-आदि। युद्ध के समय जहाँ आसुरिक शक्तियाँ सामने खड़ी हों और दैवी शक्तियों को पराजित करने के लिए तत्पर हों, वहाँ अर्जुन यदि कहे कि मेरे लिए तो कौरव और पांडव सब समान हैं क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ और इन सब को भी आत्मा के रूप में देखता हूँ, मुझे बाकी चीजों से क्या मतलब है, मुझे तो भगवान् का भजन करना चाहिए, तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता। जब लोग नैतिकता की बात करते हुए कहते हैं कि हमें तो सबसे प्रेम है, हमारी दृष्टि में तो सभी समान हैं इसलिए हम तो किसी प्रपंच में नहीं पड़ते तब हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों के अन्दर दूसरों के प्रति थोड़ी-बहुत सहानुभूति हो परन्तु वास्तव में ऐसे लोग निरे अज्ञानी ही होते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान आने पर ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहता।
अब प्रश्न उठता है कि गीता जिस समता की ओर इंगित कर रही है उसमें होने पर व्यक्ति को जब सबमें परमात्मा दिखाई देते हों तब उसे चीजें कैसी नजर आती होंगी और सभी के साथ वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा? क्योंकि इन विषयों में किसी मानसिक दृष्टिकोण से कोई लाभ नहीं होता। किसी प्रकार के मानसिक सिद्धांत के आधार पर हमें इस विषय में कोई सहायता नहीं मिलती कि दूसरों के साथ हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये। इसलिए दूसरों के साथ जीवन में हम कैसा व्यवहार करें, इसका सच्चा आधार क्या होना चाहिये? यदि हम उपनिषदों की वाणी को मानते हैं कि केवल एक परमात्मा की ही सत्ता है और वे ही सबमें अभिव्यक्त हो रहे हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, सबमें ब्रह्म है, सारे मनुष्य भगवान् के चलाए हुए ही चल रहे हैं, तो इन सब बातों का व्यावहारिक स्वरूप और इनके क्रियान्वयन का आधार क्या होना चाहिये? अर्जुन के पास तो भगवान् स्वयं रथ में विराजमान थे और उसका दिशानिर्देश कर रहे थे परन्तु सामान्य व्यक्ति को तो यह परम सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। यदि व्यक्ति को सशरीर गुरु की उपस्थिति का परम सौभाग्य प्राप्त हो तब तो फिर व्यवहार के किन्हीं बाहरी मानदंडों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती क्योंकि गुरु का वचन ही परम विधान होता है। जैसे कि, जो लोग श्रीमाताजी के पास रहते थे उन्हें किन्हीं भी निर्णयों के लिए किन्हीं बाहरी आधारों की आवश्यकता नहीं थी। क्या करना है और कैसे करना है उसका निर्देश तो श्रीमाताजी से प्राप्त हो जाता था और जो वे कहती थीं वही अंतिम निर्णय होता था। इसलिये इसमें व्यक्ति पर स्वयं निर्णय करने का किसी प्रकार का कोई भार नहीं रह जाता था। परन्तु आम व्यक्ति के लिए अपने दैनिक कार्य-व्यवहार में किसी सही मार्गदर्शन तथा व्यवहार के किसी उचित विधान की समस्या बनी रहती है। इसके समाधान के रूप में बहुतों का कहना है कि सबसे प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। परन्तु बाह्य रूप से तथाकथित प्रेम का व्यवहार और अन्तर में प्रेम का अनुभव दो भिन्न चीजें हैं। भगवान् द्वारा बहुत से असुरों और राक्षसों का संहार किये जाने पर भी हमारे ऋषि-मुनि और हमारे सभी सद्ग्रंथ यही कहते हैं कि भगवान् ने उनका उद्धार कर दिया और उन्हें वह गति प्रदान की जो किन्हीं नियम और व्रतों को पालन करने वाले सात्त्विक व्यक्ति के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए हमें क्या करना चाहिये इस बात का व्यावहारिक मार्गदर्शन हमें न तो किन्हीं नैतिक विधानों से प्राप्त होता है, न किन्हीं शास्त्रों से, न किन्हीं तथाकथित परोपकारिता या हितैषिता के विचारों से। क्योंकि वास्तव में तो नैतिकता, परोपकारिता, हितैषिता, प्रेम आदि ऐसी चीजें हैं जिनका बाहरी रूप से कोई मानदंड स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिये सच्चे व्यवहार के मानक स्थापित करने की समस्या बनी ही रहती है। और व्यक्ति जितने ही अधिक मानसिक मानक स्थापित करता है उन्हें लागू करने में वह उतनी ही अधिक पीड़ा भोगता है।
इसलिये श्रीअरविन्द वर्तमान प्रसंग का उपयोग कर इस ओर ध्यान दिला रहे हैं कि व्यक्ति बाहरी रूप से व्यवहार का कोई मानक स्थापित नहीं कर सकता। सही क्रिया तो तभी होगी जब व्यक्ति स्वयं परमात्मा बन जाएगा क्योंकि भगवान् जो करते हैं वही सही है। सही की परिभाषा भी वही है। सत्य क्या है और क्या नहीं वह तो परमात्मा की क्रिया से हो निर्धारित होता है और वे स्वयं तो सत्य से भी परे हैं। इसलिए उन पर कोई भी मापदण्ड लागू नहीं हो सकता। जब हम परमात्मा की ओर बढ़ना प्रारम्भ करते हैं तो धीरे-धीरे हमारी सभी क्रियाएँ अपने आप ही ऊपर उठने लगती हैं। चूंकि हमारा क्रमविकास चल रहा है, तो उसमें यदि हम कोई कृत्रिम या प्रचलित मापदण्ड लागू कर दें कि सबसे प्रेम करना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए आदि, तो यह अधिक समय तक टिक नहीं सकता क्योंकि हमें वास्तव में पता ही नहीं है कि किस समय, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी पर तो उन असीम परमात्मा के परम् रूप की अभिव्यक्ति होनी है और इसे किसी भी मानसिक आदर्श की सहायता से समझा ही नहीं जा सकता।
अभी तक समाज में जितने भी आदर्श लागू किए गए हैं वे केवल ऐसे पथसंकेतों के रूप में ही रहे हैं जो मनुष्य को उसकी पाशविक प्रकृति से कुछ ऊपर उठाने में उसकी सहायता करते हैं और ये इस तरीके के सामूहिक और सार्वभौमिक मानक या आदर्श के रूप में होते हैं जो मनुष्यों को एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाने से रोकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को इन मानसिक आदर्शों से कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। बड़ी-से-बड़ी नैतिकता भी व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। बड़े-से-बड़ा ब्रह्मज्ञान भी जैसे ही हमारे मन के सम्पर्क में आता है या कहें कि मन के द्वारा जिस प्रकार समझा जाता है वह हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। यदि हम उसके मापदण्डों को जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी प्रकृति में जो जगदम्बा विराजमान हैं, जो हमें कदम-कदम पर चलाती हैं, वे इन मानदण्डों को हजारों बार तोड़ देंगी। इसलिये आध्यात्मिक जीवन में ये आदर्श कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकते। आंतरिक चीजों का तथा आत्मा का अपना ही निराला विधान है जो किन्हीं भी मानसिक सूत्रों से बिल्कुल परे है और जितना ही अधिक हम उस पर हमारे कृत्रिम सिद्धांत लादने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक हम अपनी आत्मा के विधान का निषेध कर अपने-आप को संकट की स्थिति में डालेंगे। आत्मा का विधान नैतिक या अनैतिक नहीं बल्कि मन-बुद्धि से बिल्कुल परे है। इसलिए संभव है कि व्यक्ति आत्मा की प्रेरणा से सही कर्म कर रहा हो, परंतु उस विधान को समझना तो उसके लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि वह विधान समझ का विषय ही नहीं है।
इसलिये इसके अंदर व्यावहारिक मनोभाव तो यह है कि जो कुछ घटित हो चुका होता है वह भले हमें अपनी बुद्धि से कैसा भी क्यों न प्रतीत होता हो, परंतु वह सदा सर्वश्रेष्ठ ही होता है क्योंकि जगदंबा की क्रिया सदा सर्वश्रेष्ठ ही होती है। इसलिए सिद्धांततः तो सब कुछ सर्वश्रेष्ठ ही हो रहा है परंतु चूंकि यह एक क्रमविकासमय जगत् है और इसमें चीजें स्थैतिक नहीं गतिशील होती हैं, इसलिए जब उत्तरोत्तर विकास चल रहा है तो इसमें हमारी भावनाएँ, हमारे विचार, हमारी धारणाएँ, हमारे नैतिकता-अनैतिकता के सिद्धांत आदि भावी विकास को और भावी घटनाक्रम को बदलने के लिए श्रीमाँ के साधन होते हैं। इस दृष्टिकोण से सभी चीजों का अपना महत्त्व है। जो कुछ घटित हो चुका है वह तो निश्चित रूप से सर्वोत्तम ही घटित हुआ है परंतु ऐसा दृष्टिकोण हम चीजों के घटित होने के बाद ही अपना सकते हैं, उससे पूर्व नहीं। क्योंकि चीजों के घटित होने से पूर्व - जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है - हमारे विचार, भावनाएँ, कामनाएँ आदि और इन सब से अधिक सतत् चुनाव करने वाली हमारी सचेतन इच्छाशक्ति, श्रीमाँ के वे शक्तिशाली साधन हैं जो उस चीज को घटित करते हैं जो कि सर्वोत्तम है। यदि हम इस प्रकार के सचेतन चुनाव से इनकार करते हैं- इस प्रकार की मानसिक धारणा की छाया में कि सब कुछ सदा ही श्रेष्ठ होता है - तो जिस हद तक हम ऐसा करते हैं उस हद तक हम श्रीमाँ के काम में अपना सहयोग सीमित कर देते हैं। एक अवस्था के बाद जब व्यक्ति सचेतन रूप से आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है तब उसे महसूस होने लगता है कि उसके सारे क्रियाकलाप ऐसे होंगे जो श्रीमाताजी के कार्य के लिए आवश्यक हैं। वह जो भूलें करता है वे भी उसे कुछ पाठ सिखाने के लिए ही होती हैं। और ज्यों-ज्यों व्यक्ति अधिकाधिक जगदंबा की शक्ति के प्रति अपने-आप को खोलता जाएगा त्यों ही त्यों उनकी क्रिया उसमें अधिक सुचारू रूप से होने लगेगी और उसके कर्म भी अधिकाधिक उनकी क्रिया के अनुकूल और उसमें सहयोगी होंगे। और तब व्यक्ति पाएगा कि सारे बाहरी मापदंड बिल्कुल बेकार हैं। और पहले जो चीजें विकास में सहायक थीं वे ही बाद में बंधनस्वरूप लगने लगती हैं और व्यक्ति को उन सब को छोड़ देना होता है, उन्हें नष्ट कर देना होता है। इसीलिये गीता अपनी सारी शिक्षा देने के बाद कहती है कि 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' क्योंकि अर्जुन की चेतना अब इस स्तर तक विकसित हो चुकी होती है कि वह सारे धर्मों को अर्थात् सभी मानसिक मापदंडों को त्याग देने के लिए परिपक्व हो जाता है। वास्तविक स्थिति तो वह है कि व्यक्ति इस सीमा तक दिव्य जननी को दिया जा चुका हो कि उन्हें अपनी क्रिया के लिए व्यक्ति की मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक संरचनाओं की अनुमति की आवश्यकता न हो। फिर व्यक्ति के सारे क्रिया-कलाप अधिक गहरे रूप से श्रीमाताजी से जुड़ जाएँगे।
परंतु बाहरी क्रिया तथा लक्षणों के आधार पर तो आवश्यक नहीं कि हम अपने सामने खड़े परमात्मा तक को भी पहचान सकें। हमारे सामने परमात्मा के अवतार उपस्थित हों और फिर भी आवश्यक नहीं कि हम उन्हें उनके कर्मों से पहचान पाएँ। जब अर्जुन ही श्रीकृष्ण को नहीं पहचान पाया तब दूसरों की तो बात ही क्या है। यह पहचान किन्हीं भी बाहरी तरीकों से नहीं की जा सकती। यह केवल भीतर से ही हो सकती है।
II. निर्वाण तथा संसार में कर्म
ज्ञानमार्ग का एकांगी रूप से अनुसरण करनेवाले संकीर्ण सिद्धान्त की तरह केवल अक्षर पुरुष के साथ एक हो जाना ही नहीं, अपितु समग्र सत्ता के योग द्वारा जीव का पुरुषोत्तम के साथ एक हो जाना ही गीता की संपूर्ण शिक्षा है।....परन्तु पुरुषोत्तम के साथ एकता स्थापित करने का सीधा रास्ता अक्षर पुरुष की सुदृढ़ अनुभूति में से होकर ही है, और इस पर गीता ने पहली आवश्यकता बताकर बहुत बल दिया है, केवल जिसके बाद ही कर्म और भक्ति अपना संपूर्ण दिव्य महत्त्व या अर्थ प्राप्त करते हैं, इसी कारण हम गीता के आशय को समझने में भूल कर जाते हैं। क्योंकि यदि हम केवल उन्हीं श्लोकों को देखें जिनमें इस आवश्यकता पर अत्यंत बलपूर्वक आग्रह किया गया है और गीता के विचारों के उस संपूर्ण क्रम पर ध्यान देने में लापरवाही करें जिस क्रम में ये विचार आए हैं, तो अनायास ही इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि गीता वास्तव में कर्महीन लय को जीव की अंतिम स्थिति के रूप में और कर्म को अविचल अक्षर पुरुष की स्थिरता की ओर प्राथमिक साधन मात्र के रूप में प्रतिपादित करती है। पाँचवें अध्याय के अन्त में और छठे अध्याय में सर्वत्र यही आग्रह अत्यंत प्रबल और व्यापक है। वहाँ हम एक ऐसे योग का वर्णन पाते हैं जो प्रथम दृष्टि में कर्ममार्ग से विसंगत प्रतीत होगा और वहाँ हम बारंबार निर्वाण शब्द का प्रयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया गया पाते हैं जिस पद को योगी प्राप्त करता है।
गीता में अक्षर पुरुष की अविचलता और समानता की जो बातें कही गई हैं वे तो साधना में केवल शुरुआती चीजें हैं, अधिकांश लोग इसी को गीता की अंतिम शिक्षा समझकर इसके आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो कि मूढ़ता है। क्योंकि इनका निरूपण करने के बाद गीता कर्मयोग, ज्ञानयोग और इनकी पराकाष्ठा के रूप में भक्तियोग के गंभीरतर विषयों का निरूपण करती है। इसलिये श्रीअरविन्द यहाँ हमें सचेत करते हैं कि गीता के अध्ययन में हमें यह सावधानी बरतनी चाहिये कि उसके श्लोकों को संपूर्ण कलेवर से अलग हटाकर न लें बल्कि उसकी संपूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखकर एक उचित परिप्रेक्ष्य में ही लें अन्यथा गीता की शिक्षा को समग्रता से नहीं समझ पाएँगे। हमें यह देखना होगा कि गीता क्षर और अक्षर से होते हुए किस प्रकार पुरुषोत्तम तत्त्व की ओर अपनी शिक्षा को विकसित कर रही है। यदि अक्षर ब्रह्म ही अंतिम स्थिति हो और कर्म उस स्थिति तक पहुँचने के लिए साधन मात्र ही हों, तब तो फिर एकमात्र उद्देश्य रह जाता है कि व्यक्ति यथासंभव और यथाशीघ्र कर्मों का त्याग कर के अक्षर ब्रह्म की शांति में लीन हो जाए। और एक बार अक्षर ब्रह्म की शांति और समता में लीन होने पर फिर व्यक्ति के लिए कोई कर्म नहीं बचता। पर तब तो प्रेम का, हृदय के भाव का, भक्ति का तो कोई स्थान ही नहीं रह जाता। जबकि गीता तो भक्तियोग को कर्म और ज्ञान की पराकाष्ठा के रूप में प्रतिपादित करती है। इसलिए यदि हम अक्षर ब्रह्म को प्रतिपादित करने वाले श्लोकों को ही गीता का अंतिम वचन मान बैठें तो यह गीता की संपूर्ण शिक्षा को एकांगी या फिर अधूरे रूप से ही देखना हुआ।
इस पद या स्थिति का लक्षण है निर्वाण की परम् शान्ति, शान्तिं निर्वाणपरमां, और मानो इस बात को सर्वथा स्पष्ट करने के लिए कि यह निर्वाण बौद्धों का शून्य में, अर्थात् अपनी सत्ता के आनंददायक निषेध में, निर्वाण नहीं है अपितु आंशिक सत्ता का पूर्ण सत्ता में वेदान्तिक लय है, गीता ने सदा 'ब्रह्म-निर्वाण' शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है ब्रह्म में विलीन होना; और 'ब्रह्म' शब्द से यहाँ अभिप्राय अवश्य ही अक्षर ब्रह्म से प्रतीत होता है, कम-से-कम मुख्यतः उस अंतःस्थ कालातीत आत्मा को द्योतित करने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है जो बाह्य प्रकृति में व्याप्त या अंतर्निहित होते हुए भी सक्रिय रूप से उसमें कोई भाग नहीं लेती। इसलिये हमें यह देखना होगा कि गीता का यहाँ अभिप्राय किस ओर है, और विशेषकर यह कि यह शान्ति क्या पूर्ण नैष्कर्म्य की शान्ति ही है, तथा क्या अक्षर ब्रह्म में निर्वाण होने का अभिप्राय क्षर के सम्पूर्ण ज्ञान तथा चेतना का तथा क्षर में होनेवाले सम्पूर्ण कर्म का पूर्ण उन्मूलन ही है? निश्चय ही हम निर्वाण तथा किसी प्रकार के जगत्-अस्तित्व और कर्म को एक-दूसरे से सर्वथा विसंगत मानने के अभ्यस्त हैं और यहाँ तक तर्क दे डालने की प्रवृत्ति रख सकते हैं कि 'निर्वाण' शब्द का प्रयोग ही अपने आप में पर्याप्त है और इस विवाद का निर्णय कर देता है। परन्तु यदि हम बौद्ध मत का ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो हमें यह सन्देह होगा कि क्या यह पूर्ण विसंगतता बौद्धों तक के लिए भी यथार्थतः थो या नहीं; और यदि हम गीता को ध्यान से देखें तो हम पाएँगे कि यह विरोध या विसंगतता वेदान्त की इस परम् शिक्षा के अन्दर नहीं है।
'ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः' अर्थात् ब्रह्मचेतना में पहुँचे हुए ब्रह्मविद् की पूर्ण समता की चर्चा करने के बाद उसके बाद के नौ श्लोकों में गीता ने ब्रह्मयोग और ब्रह्मनिर्वाण-संबंधी भाव को विस्तार के साथ कहा है।
बाह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ।। २१ ।।
२१. जब जीव और अधिक बाह्य विषयों के स्पशों में आसक्त नहीं होता, तब वह आत्मा में जो सुख विद्यमान है उसे प्राप्त करता है; ऐसे मनुष्य का आत्मा योग के द्वारा ब्रह्म के साथ युक्त होने के कारण अविनाशी सुख का लाभ करता है।
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ।। २२ ।।
२२. बाह्य पदार्थों के (इन्द्रियों के साथ) स्पशौँ से उत्पन्न होनेवाले जो सुखभोग हैं वे केवल दुःख का कारण होते हैं; उनका आरंभ और अन्त होता है; इसलिये, हे कौन्तेय! ज्ञानी उनमें आनन्द (सुख) का अनुभव नहीं करता।
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥
२३. जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले यहाँ पृथ्वी पर शरीर में रहते हुए ही काम और क्रोध के वेग (तीव्रता) को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी है, वह सुखी मनुष्य है।
गीता कहती है कि काम-क्रोध और आवेग के आक्रमणों से मुक्त होने के लिए अनासक्त होना अत्यावश्यक है, एक ऐसी मुक्ति जिसके बिना सच्चा सुख सम्भव नहीं है। वह सुख और वह समत्व, मनुष्य को शरीर में रहते हुए हो पूर्ण रूप से प्राप्त करने होंगे; निम्न विक्षुब्ध प्रकृति के जिस दासत्व के कारण वह यह समझता था कि पूर्ण मुक्ति शरीर को छोड़ने के बाद ही प्राप्त होगी, उस दासत्व का लेशमात्र भी उसके अन्दर नहीं रह जाना चाहिए: इसी जगत् में, इसी मानव-जीवन में अर्थात् देह त्याग करने से पहले ही 'प्राक् शरीर-विमोक्षणात्' पूर्ण आध्यात्मिक स्वातंत्र्य लाभ करना और भोगना होगा।
योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः ।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।। २४।।
२४. वह जिसे आंतरिक सुख और आंतरिक आराम-विश्राम और आंतरिक प्रकाश प्राप्त है, वह योगी ब्रह्म हो जाता है और ब्रह्म में निर्वाण को प्राप्त हो जाता है।
यहाँ स्पष्ट रूप से निर्वाण का अर्थ है उस उच्चतर आध्यात्मिक, अंतरात्मा, में अहंकार का लोप होना जो सदा देशकालातीत, कार्य-कारणबंधनातीत तथा क्षरणशील जगत् के परिवर्तनों से अबद्ध है और जो सदा आत्मानन्दमय, आत्मप्रकाशमय और नित्य-शान्तिमय है। वह योगी अब अहंकारस्वरूप नहीं रह जाता, ऐसा छोटा-सा व्यक्तित्व नहीं रह जाता जो मन और शरीर से सीमित हो; वह ब्रह्म हो जाता है; उसकी चेतना शाश्वत पुरुष की उस अक्षर दिव्यता के साथ एक हो जाती है जो उसकी प्राकृत सत्ता में व्याप्त है।
परन्तु क्या यह लौकिक-चेतना से दूर, समाधि की किसी गहरी निद्रा में चले जाना है, अथवा क्या यह प्राकृत सत्ता तथा व्यष्टि पुरुष के किसी ऐसे परम् ब्रह्म (पुरुष) में लय हो जाने या मोक्ष पाने की तैयारी है जो सर्वथा और सदा प्रकृति और उसके कर्मों से परे है? क्या निर्वाण को प्राप्त होने के पहले लौकिक-चेतना से संबंध-विच्छेद आवश्यक है, अथवा क्या निर्वाण जैसा कि उस प्रकरण से मालूम होता है, एक ऐसी अवस्था है जो लौकिक-चेतना के साथ-साथ रह सकती और अपने ही तरीके से उसका अपने अन्दर समावेश भी कर सकती है? यह बाद वाले प्रकार की अवस्था हो स्पष्ट रूप से गीता द्वारा अभिप्रेत मालूम होती है, क्योंकि इसके बाद के ही श्लोक में गीता ने कहा है कि...
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।
छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।। २५।।
२५. जिनके पापरूप मल धुल गये हैं, जिनकी संशयरूप ग्रन्थि कट गयी है, जिन्होंने अपने आत्मा (मन, इन्द्रिय आदि) को अपने वश में किया है, जो समस्त प्राणियों के हितसाधन में लगे रहते हैं ऐसे ऋषि ब्रह्म में निर्वाण को प्राप्त होते हैं।
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ।। २६।।
२६. जो काम और क्रोध से मुक्त हो गये हैं और जिन्होंने अपने चित्त को संयत किया है (आत्मप्रभुत्व प्राप्त किया है), ऐसे यतियों (जो योग और तपस्या के द्वारा आत्मसंयम का अभ्यास करते हैं) के सब ओर ब्रह्म में निर्वाण रहता है, उन्हें परिव्याप्त किये रहता है, वे पहले ही उसमें निवास करते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान होता है।
ब्रह्मनिर्वाण कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तब प्राप्त हो जब व्यक्ति शरीर का त्याग कर देता है। पार्थिव जगत् में रहते हुए भी जब व्यक्ति उस ब्रह्म चेतना में प्रवेश करता है तब उसे अपने चारों ओर ही उस निर्वाण का अनुभव तथा आस्वादन प्राप्त होता है। यदि ब्रह्मनिर्वाण शरीर रहते संभव न हो और उसके लिए इस देह को त्याग देना आवश्यक हो तब तो फिर अर्जुन को उस निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करने के लिए देह को त्याग देना होगा। यदि ऐसा हो तब तो गीता की शिक्षा तो बहुत ही भ्रांत प्रकार की व ऐसी हुई जो अपना ही खंडन करती है। इसलिए यह स्पष्ट ही है कि निर्वाण तो चेतना की एक ऐसी स्थिति है जो देह में रहते हुए ही प्राप्त की जा सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि यह निर्वाण योग की कोई बहुत ऊँची स्थिति हो। क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त होने पर श्रीभगवान् अर्जुन को कहते हैं कि अब मेरे पास आ जा क्योंकि उस ब्रह्म का आधार भी मैं ही हूँ। इसलिए मेरी भक्ति करने से तू ब्रह्म के भी परे चला जाएगा। परंतु चूंकि अर्जुन ने अपनी परंपरा से ये बातें सुन रखी थी कि निर्जन वनों में जाकर या हिमालय में जाकर तप करने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान् उसकी बुद्धि में प्रकाश लाने के लिए, उसकी पूर्वधारणाओं को तोड़ने तथा उसे आगे ले जाने के लिए स्पष्ट कर रहे हैं कि जो उस चेतना में पहुँच गया है उसके लिए तो चारों ओर निर्वाण ही निर्वाण है। इस बात से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस ब्रह्मनिर्वाण को लोग अंतिम चीज या फिर अंतिम उद्देश्य मान बैठते हैं वह तो केवल एक आरंभिक सोपान ही है। क्योंकि कर्मों का त्याग कर वन में जाकर साधना कर के ब्रह्म को प्राप्त करना ही यदि गीता की शिक्षा का सार होता तो अर्जुन तो पहले ही उसके लिए तैयार था। तब तो शेष गीता को विकसित करना और उसे युद्ध में प्रवृत्त करना एक असंगत बात होती। जब हमें इन बातों के पीछे का रहस्य समझ में आता है तभी हम सच्चे रूप से समझ पाते हैं कि जो अकर्म का उपदेश कर रहे हैं कैसे वे ही घोर कर्म को संपादित करते हैं और जो संसार के मोह को त्यागने की बात करते हैं वे ही श्री शंकराचार्य अपनी माता के अंतिम संस्कार करने के लिए प्रस्तुत होते हैं।
अर्थात् आत्मा का ज्ञान होना और आत्मवान् होना ही निर्वाण में रहना है। यह स्पष्ट ही निर्वाण के विचार का एक व्यापक विस्तार रूप है। काम- क्रोधादि दोषों के सभी दाग-धब्बों से मुक्ति, और यह मुक्ति जिस समत्व-बुद्धि के आत्म-प्रभुत्व पर आधारित है वह, सब भूतों के प्रति समत्व, सब के प्रति कल्याणकारी प्रेम, अज्ञानजनित उस संशय और अंधकार का अंततः नाश जो सर्व-एकीकारी भगवान् से और हमारे अन्दर और सबके अन्दर जो 'एक' आत्मा है उसके ज्ञान से हमको अलग रखता है, ये सब स्पष्ट ही निर्वाण की अवस्थाएँ हैं जो गीता के इन श्लोकों में प्रतिपादित की गयी हैं, इन्हीं से निर्वाण-पद सिद्ध होता है और ये ही उसके आध्यात्मिक तत्त्व हैं।
इस प्रकार निर्वाण लौकिक-चेतना और संसार के कर्मों के साथ स्पष्टतः संगत है। क्योंकि जो ऋषि निर्वाण को प्राप्त हैं वे इस क्षर जगत् में भगवान् के विषय में सचेतन हैं और कर्मों के द्वारा उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाये रखते हैं; वे सब भूतों के कल्याण में लगे रहते हैं सर्वभूतहिते रता... संसार में कर्म करना ब्रह्म में निवास करने की स्थिति से बेमेल नहीं है, उल्टे यह तो उस स्थिति की अपरिहार्य शर्त और बाह्य परिणाम है, क्योंकि जिस ब्रह्म में निर्वाण लाभ किया जाता है, जिस आध्यात्मिक चेतना में हमारा पृथक् अहंभाव विलीन हो जाता है, वह न केवल हमारे अन्दर ही है, अपितु इन सब भूतों में भी है; वह इन सब जगत्-प्रपंचों से केवल पृथक् और इनके ऊपर ही नहीं है, अपितु इन सबमें व्याप्त है, इन्हें धारण किये हुए है और इनमें विस्तारित है..
परन्तु तुरंत इसके बाद ही फिर दो श्लोक हम ऐसे पाते हैं जो इस निष्कर्ष से दूर ले जाते प्रतीत हो सकते हैं।
स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्वक्षुचैवान्तरे ध्रुवोः ।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।। २७।।
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ।। २८।।
२७-२८. बाहरी पदार्थों के समस्त स्पर्शों को अपने से बाहर कर के और दृष्टि को ध्रुवों के बीच में स्थिर कर के, नासिका के छिद्रों में गति करनेवाले प्राण और अपान वायु को सम कर के जिसने इन्द्रिय, मन और बुद्धि को संयत किया है, जिससे कामना, भय और क्रोध दूर हो गये हैं ऐसा जो मोक्ष में लगा हुआ मुनि है वह सर्वदा मुक्त ही है।
यहाँ हम योग की एक ऐसी प्रणाली को पाते हैं जो एक ऐसे तत्त्व को ले आती है जो कर्मयोग से और यहाँ तक कि उस विशुद्ध ज्ञानयोग से भी भिन्न प्रतीत होता है जो विवेक और ध्यान से साधित होता है; यह तत्त्व अपने सभी लक्षणों से राजयोग की प्रणाली से संबद्ध है और राजयोग की मनो-भौतिक तपस्या को प्रस्तावित करता है। इसमें मन की सभी प्रवृत्ति पर विजय 'चित्तवृत्तिनिरोध' है; इसमें श्वास पर नियंत्रण 'प्राणायाम' है; इसमें इंद्रियों और दृष्टि को भीतर खींचना है। ये सब आंतरिक समाधि की ओर ले जानेवाली प्रक्रियाएँ हैं, इन सबका लक्ष्य मोक्ष है और सामान्य व्यवहार की भाषा में मोक्ष कहते हैं, केवल पृथक्कारी अहं-चेतना के त्याग को ही नहीं, अपितु संपूर्ण सक्रिय कर्म-चेतना के त्याग को भी, परब्रह्म में अपनी सत्ता के संपूर्ण अस्तित्व का लय कर देने को। तो क्या हम यह समझें कि गीता ने यहाँ इसका विधान इस अभिप्राय से किया है कि इसी लय को मुक्ति का चरम उपाय मानकर ग्रहण किया जाए या इस अभिप्राय से कि यह बहिर्मुख मन को वश में करने का केवल एक विशिष्ट उपाय तथा एक शक्तिशाली साधन मात्र है? क्या यही आखिरी बात, परम् वचन या महावाक्य है? हम इसे दोनों ही मान सकते हैं, एक विशेष उपाय, एक विशिष्ट साधन भी और कम-से-कम चरम गति का एक द्वार भी; अवश्य ही इस चरम गति का साधन लय हो जाना नहीं है, अपितु विश्वातीत सत्ता में ऊपर उठ जाना है। क्योंकि यहाँ इस श्लोक में भी जो कुछ कहा गया है वह अंतिम वाक्य नहीं है; महावाक्य, आखिरी बात, परम् वचन तो इसके बाद के श्लोक में आता है जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है।
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।। २९।।
२९. जब मनुष्य मुझे यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता के रूप में, समस्त लोकों के महान् ईश्वर के रूप में, समस्त प्राणियों के सुहृद के रूप में जान लेता है, तब वह शान्ति को प्राप्त हो जाता है।
जैसा कि श्रीअरविन्द ने स्पष्ट कर ही दिया है और जो लोग साधना करते हैं उनमें से अधिकांश यह जानते भी हैं कि साधना में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वह है चित्त की वृत्तियों और प्राण के आवेगों से उठने वाली चंचलताओं की। हालाँकि प्राण के नियमन के लिए प्राणायाम देखने में तो एक बहुत ही यांत्रिक उपाय प्रतीत होता है परंतु है बहुत ही कारगर। और जो भी इसे करता है वह पाता है कि इसे करने से प्राण की चंचलताओं में बहुत कुछ नियमन आ जाता है। पतंजलि के सूत्रों के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा व्यक्ति अपनी चंचल मन, प्राण और शरीर की वृत्तियों से समाधि की अवस्था तक पहुँचता है जिसमें कि प्राणायाम चौथी अवस्था है जो कि बाकी चार में सहायता पहुँचाती है। परंतु अपनी वर्तमान पाशविक प्रकृति को देखते हुए प्रतीत होता है कि केवल यम और नियम को ही जीवन भर अभ्यास कर के सिद्ध कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए लगभग असंभव ही है। इसलिए परिपाटी यह थी कि लोग संसार का त्याग कर वनों में चले जाते थे जहाँ फिर बाहरी कामनाएँ अधिक हावी नहीं होती थीं और इनका अभ्यास करना अधिक आसान हो जाता था। हालाँकि आवश्यक नहीं है कि इससे भी यम-नियम पूर्णतः सिद्ध हो जाएँ, परंतु फिर भी कुछ हद तक तो इनका अभ्यास हो ही जाता था। इसके बाद आसन और प्राणायाम के माध्यम से जब व्यक्ति प्राण और शरीर का अधिक नियमन कर लेता है तब उसका प्राण अधिक परिष्कृत और सूक्ष्म बन जाता है और व्यक्ति भौतिक चेतना से ऊपर उठ जाता है जिसके बाद उसे अनेकों अनुभव होने आरंभ हो जाते हैं। परंतु इस सब को श्रीअरविन्द ने अपनी योग पद्धति में कोई अधिक ऊँचा स्थान नहीं प्रदान किया। वे अपनी योग पद्धति में भगवान् के प्रति पूर्ण समर्पण पर ही बल देते हैं और इन सभी प्रचलित प्रणालियों को इस रूप में मानते हैं कि इनका अभ्यास व्यक्ति अपनी साधना की किसी स्थिति विशेष में और किसी समय विशेष पर और वह भी यदि आवश्यक हो तो कर सकता है और किस मात्रा में इनका अभ्यास करना है यह भी उसे अपनी अंतरात्मा की आवश्यकता के अनुसार तय करना होता है। क्योंकि श्रीअरविन्द कहते हैं कि अपने आप में इन सभी योग-प्रणालियों का अभ्यास मनुष्य को अतिशय अहंकार से भर सकता है। हमारे प्राचीन साहित्य में अनेकों उदाहरण दिये जाते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति सिद्धियों के प्राप्त होने पर अहंकार से भर जाता है और तब भगवान् की कृपा से उसके अहंकार को यथा-तथा भंग भी किया जाता है। सामान्यतया योग की इन प्रणालियों को साधना का पर्याय समझ लिया जाता है जबकि आवश्यक नहीं है कि सच्ची आंतरिक साधना में इनका कोई विशेष सकारात्मक योगदान भी हो। यम-नियमादि प्रणालियाँ तो मात्र एक माध्यम हैं जो किन्हीं लोगों के लिए उनकी साधना के अंदर - और वह भी उनके गुरु के परामर्श के अनुसार और उनकी देखरेख में - सहायक सिद्ध हो सकती हैं। हाँ, इन प्रणालियों के अभ्यास से मनुष्य को सूक्ष्म लोकों के अनुभव होने लगते हैं। परंतु श्रीमाताजी के अनुसार इसमें खतरा यह रहता है कि अधिकांशतः व्यक्ति अपने ही मनोनिर्मित तथा आत्मपरक जगतों में निवास करने लगता है और वास्तविक जगत् से उसका संबंध-विच्छेद होता जाता है। इसलिये श्रीअरविन्द कहते हैं कि यह व्यक्ति की अंतरात्मा के गठन पर निर्भर करता है कि उसके लिये कौनसी पद्धति उचित होगी क्योंकि अपने-आप में तो कोई भी पद्धति उचित या अनुचित नहीं होती। कोई पद्धति किसी के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है और किसी के लिए बड़ी ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। यहाँ तक कि व्यक्ति-विशेष के लिए जो पद्धति किसी एक समय लाभदायक सिद्ध होती है वह आवश्यक नहीं कि बाद में भी वैसी रहे। इसीलिए हमारी संस्कृति में सभी चीजों के लिए देश, काल और पात्र पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसीलिये श्रीअरविन्द कहते हैं कि वास्तव में तो हमारी साधना हमारे प्रयासों के कारण नहीं बल्कि उनके बावजूद ही होती है। क्योंकि साधना के सभी प्रयास तो उस आंतरिक सत्ता के दबाव के कारण उठने वाली केवल बाहरी प्रतिक्रियाएँ मात्र हैं जो उस सत्ता की उपस्थिति को सूचित करती हैं। और साधना का वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति की वही सच्ची सत्ता बाहर आकर उसके सभी हिस्सों पर अधिकार करे और अपने-आप को अभिव्यक्त करे। इसलिये श्रीअरविन्द के अनुसार, "व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है और मन तथा बुद्धि में आलोक प्राप्त कर सकता है; वह शक्ति आयत्त कर सकता है और प्राण के अन्दर सभी प्रकार की अनुभूतियों का आनन्द भोग सकता है; यहाँ तक कि व्यक्ति आश्चर्यजनक भौतिक सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकता है; परंतु पीछे अवस्थित अन्तरात्मा की सच्ची शक्ति, यदि प्रकट नहीं होती, यदि चैत्य प्रकृति सम्मुख नहीं आती तो फिर अभी तक कुछ भी वास्तविक कार्य नहीं हुआ है। ... यदि बौद्धिक ज्ञान या मानसिक विचारों या किसी प्राणिक कामना के प्रति आसक्ति होने के कारण चैत्य चेतना में नवजन्म लेना अस्वीकार हो, यदि श्रीमाताजी का नवजात बालक बनना अस्वीकार हो, तो साधना में असफलता ही होगी।" (CWSA 30, p. 337-38)
प्राणायाम आदि प्रणालियों के द्वारा इतना अवश्य हो जाता है कि व्यक्ति को सूक्ष्म जगतों के अनुभव होने के कारण उसकी इस जड़भौतिक जगत् से अतिशय आसक्ति कुछ कम हो जाती है और उसे यह भान हो जाता है कि इसके अतिरिक्त और इससे विशालतर तथा भव्यतर जगतों का भी अस्तित्व है। इस दृष्टिकोण से ये प्रणालियाँ कुछ लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। परंतु यह तो केवल शुरुआत मात्र है। जब साधना में व्यक्ति अधिक आगे जाता है तब धीरे-धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जिन चीजों को लेकर उसने अपनी साधना आरंभ की थी वे भी क्रमशः छोड़नी होती हैं और फिर उसे नये सूत्रों को पकड़ना होता है। यह वैसा ही होता है मानो हमारी जंजीरें कुछ ढीली होती जा रही हों तथा हमें विचरण करने का कुछ अधिक स्थान मिल रहा हो। परंतु फिर भी जंजीरें तो रहती ही हैं। और ये जंजीरें इन पारंपरिक योग पद्धतियों के माध्यम से भी टूट सकती हैं और इनसे भिन्न अन्य तरीकों से भी टूट सकती हैं। और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी बिना किसी बाहरी पद्धति के ही जंजीरें स्वयं ही टूट जाती हैं। ये सारी बातें समझने पर ही हम गीता की शिक्षा के विकासक्रम को एक उचित परिप्रेक्ष्य में देख सकेंगे अन्यथा तो हम किसी एक शिक्षा को ही गीता का संपूर्ण सार मान बैठने की भूल कर बैठेंगे जैसा कि अधिकांशतः होता ही है। साधना में सभी अनुभवों का मूल्य व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई पर निर्भर करता है। यदि आंतरिक सच्चाई न हो तो अनुभवों की सत्यता की भी निश्चितता नहीं रहती और वे व्यक्ति के अहं को ही पोषित करने का काम करते हैं। भगवान् की अभिव्यक्ति किन्हीं ऊँचे से ऊँचे अनुभवों की भी पकड़ में नहीं आ सकती। इसलिए श्रीमाताजी कहती हैं कि साधना में व्यक्ति ध्यान के द्वारा प्रगति कर सकता है, परंतु सही भावना से कर्म कर के व्यक्ति उससे सौ गुना अधिक प्रगति कर सकता है। इसीलिए बड़े से बड़ा ज्ञान भी भगवान् की एक छोटी-सी सेवा के सामने कुछ नहीं है। जब हम इन सब चीजों को थोड़ा-थोड़ा समझने लगते हैं तभी हमें चीजें सही परिप्रेक्ष्य में समझ में आने लगती हैं और हम एकांगी रूप से किसी एक या दूसरी चीज पर ही आग्रह रखने की भूल करने से कुछ बच जाते हैं।
यहाँ कर्मयोग की शक्ति ही फिर से आ जाती है; सक्रिय ब्रह्म, विराट् पुरुष, के ज्ञान पर ज्ञानब्रह्मनिर्वाण की शान्ति की आवश्यक शर्तों के रूप में बल दिया गया है। यहाँ हम गीता के महान् भाव, पुरुषोत्तम के भाव की ओर लौटते हैं, यद्यपि यह नाम गीता के उपसंहार के कुछ ही पहले आता है, तथापि गीता में आदि से अंत तक जहाँ-जहाँ श्रीकृष्ण 'अहं', 'माम्' इत्यादि पदों का प्रयोग करते हैं वहाँ-वहाँ उनका अभिप्राय उन्हीं भगवान् से है जो हमारी कालातीत अक्षर सत्ता में हमारे एकमेवाद्वितीय आत्मस्वरूप में हैं, जो जगत् में भी अवस्थित हैं, सब भूतों में, सब कर्मों में विद्यमान हैं, जो निश्चल-नीरवता और शान्ति के अधीश्वर हैं, जो शक्ति और कर्म के स्वामी हैं, जो इस महायुद्ध में सारथी रूप से अवतीर्ण हैं, जो परात्पर पुरुष हैं, परमात्मा हैं, सर्वमिदं हैं, प्रत्येक जीव के ईश्वर हैं। वे सब यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, इसलिए मुक्तिकामी पुरुष सब कर्मों को यज्ञ और तपरूप से करे, वे सर्वलोकमहेश्वर हैं, जो इस प्रकृति तथा इन सब प्राणियों में प्रकट हुए हैं, इसलिए मुक्त पुरुष मुक्त होने पर भी, इन जगतों में लोगों का समुचित संचालन व नेतृत्व करने के लिए, लोकसंग्रहार्थ, कार्य करे; 'वे सब भूतों के सुहृद् हैं' इसलिए वही मुनि है जिसने अपने अन्दर और अपने चारों ओर निर्वाण लाभ किया है, फिर भी वह सदा सब भूतों के कल्याण में रत रहता है - जैसे बौद्धों के महायान पंथ में भी निर्वाण का परम् लक्षण जगत् के सब प्राणियों के प्रति करुणामय कर्म को ही समझा जाता है। इसीलिए अपने कालातीत अक्षर आत्मस्वरूप में भगवान् के साथ एकत्व प्राप्त कर लेने पर भी वह मनुष्य से दिव्य प्रेम करने में, भगवान् के लिए प्रेम और भक्ति करने में समर्थ होता है क्योंकि उसके अन्दर प्रकृति की क्रीड़ा के संबंध भी समाविष्ट हैं।
छठे अध्याय के आशय की तह में पहुँचने पर यह बात और भी अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि गीता के इन श्लोकों का यही तात्पर्य है। छठे अध्याय में पाँचवे अध्याय के इन्हीं अंतिम श्लोकों के भाव का विशदीकरण और पूर्ण विकास किया गया है - और इससे यह पता चलता है कि गीता इन श्लोकों को कितना महत्त्व देती है।
प्रश्न : श्रीअरविन्द की पद्धति में हम प्रायः दो प्रकार की सत्ताओं की चर्चा पाते हैं। एक क्रमविकास की प्रक्रिया से आए (evolutionary) जीव हैं और दूसरी वे सत्ताएँ हैं जो क्रमविकास से न होकर सीधे निवर्तन (involution) के द्वारा धरती पर आती हैं। तो फिर जब हम अद्वैत की बात करते हैं तो फिर ये दो प्रकार की सत्ताएँ कैसे हैं?
उत्तर : भगवान् बाध्य थोड़े ही हैं कि वे दो भिन्न कपड़े धारण न कर सकते हों, जबकि दोनों में वे हैं तो स्वयं ही। एक रूप में वे अपने को प्रकृति के अधीनस्थ कर देते हैं और दूसरे में अधीनस्थ नहीं करते। क्रमविकासमय जीव के अंदर तो उन्होंने अपनी इच्छा से अपने को सीमित किया है जबकि निवर्तन में आई सत्ताओं में वे ऐसा नहीं करते। यह वैसा ही है जैसे मानो एक स्थिति में वे अपने हाथों को बाँध कर क्रीड़ा करते हैं जबकि दूसरी अवस्था में वे अपने हाथों को खुला रखकर क्रीड़ा करते हैं चूंकि ऐसी उनके नाटक की आवश्यकता होती है। परंतु दोनों ही अवस्थाओं में वे उतने ही परमात्मा होते हैं। तो ये सभी रूप तो भगवान् की चेतना की भिन्न अवस्थाएँ मात्र हैं जिनमें किसी में भी अवस्थित होने पर भी परमात्मा उतने ही परमात्मा होते हैं। अंतर केवल उनकी अभिव्यक्ति में होता है। उनकी क्रीड़ा के लिए जैसी स्थिति आवश्यक होती है वैसी ही वे अपना लेते हैं।
प्रश्न : परंतु क्रमविकासमय जीव तो साक्षी, अनुमता आदि भावों को तो अपना सकता है परंतु ईश्वर भाव नहीं अपना सकता। ईश्वर भाव में तो केवल निवर्तित हुई या फिर अवतरित हुई सत्ताएँ ही जा सकती हैं?
उत्तर : यदि क्रमविकासमय जीव के अंदर ईश्वर भाव आना है तो वह उसके अंदर ऊपर से अवतरित होगा क्योंकि क्रमविकास से ईश्वर भाव में नहीं जाया जा सकता। क्रमविकास की प्रक्रिया का तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया में यदि जीव अनंत काल तक भी विकास करता रहेगा तो भी वह ईश्वर भाव में नहीं जा सकेगा। वह तो केवल तभी संभव है जब उसके लिए ईश्वर भाव में जाना ऊपर से नियत हो और तब ईश्वर भाव उसके अंदर अवतरित हो जाता है। मनुष्य ईश्वर चेतना का अनुभव तो प्राप्त कर सकता है परंतु उसमें ईश्वर की चेतना नहीं होती। जबकि अवतार में ईश्वर भाव होता है परंतु ईश्वर भाव होते हुए भी अपने कार्य के लिए उन्हें जितनी आवश्यकता होती है बाहरी रूप से वे केवल उतने ही सचेतन होते हैं। इस प्रकार अपने कार्य के अनुसार वे अपनी चेतना को स्वयं निर्धारित तथा सीमित कर लेते हैं। परंतु यह आत्म-सीमन होता है, कोई अयोग्यता या बाध्यता नहीं होती। गीता में भी भगवान् इस सूक्ष्म भेद को स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार वे अवतार के रूप में और साधारण जीव के रूप में भिन्न-भिन्न रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। परंतु हम अपने सीमित मानसिक उपकरण से इन विषयों को कितना भी समझने का प्रयास करें, ये उसकी पकड़ में नहीं आ सकते। हालाँकि हमारा अहंकार हमारी इस अयोग्यता को स्वीकार नहीं करता, परंतु जिस प्रकार एक पशु चेतना मानव चेतना को और उसके दृष्टिकोण से चीजों के स्वरूप को नहीं देख सकती, उसी प्रकार मानव चेतना दिव्य चेतना को और उसके नजरिये से जगत् के विषयों को नहीं समझ सकती। इसलिए मानवता की ऊँची से ऊँची उड़ान भी भगवत्ता को नहीं माप सकती। हमारे गंभीरतम अनुभव, हमारे गहनतम तत्त्वचिंतन आदि भी परम को जान नहीं सकते। भगवान् का स्वरूप तो अचिंत्य है। वे हमारे किन्हीं भी वर्णनों से अनंत रूप से परे हैं। पर क्योंकि परमात्मा स्वयं हमारे अंदर विराजमान हैं, इसलिये हम उनसे एक हो सकते हैं।
प्रश्न : भगवान् कहते हैं कि "ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति", कि केवल जान लेने भर से तुझे शान्ति प्राप्त हो जाएगी, तो केवल जान लेने भर से ही किस प्रकार शान्ति प्राप्त हो सकती है?
उत्तर : गीता केवल मानसिक विचार की बात नहीं कर रही है, वह तो जानने की बात कर रही है। किसी मानसिक विचार में और वास्तव में सच्चे रूप से जानने में अंतर है। विचार हमें जानने तक ले जा सकता है। और हो सकता है कि वह विचार किसी गहरे ज्ञान के प्रभाव से ही उठ रहा हो। ये सभी संभावनाएँ हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि वह सच्चा ज्ञान ही हो। जानने का वास्तव में अर्थ है अनुभव होना। बिना अनुभव के व्यक्ति जान नहीं सकता। परंतु अनुभव से ऊपर भी अन्य चीजें हैं। श्रीमाताजी कहती हैं कि जानना अच्छा है, उसे जीना और भी अच्छा है, पर वही बन जाना पूर्णता है और वही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसलिये ईश्वर को जानना तो अच्छा है, परंतु वास्तविक बात है स्वयं ईश्वर बन जाना। अवतारों की विशिष्टता यही है कि वे उस ईश्वर-भाव को अभिव्यक्त करते हैं। वे तो अपने बाहरी कर्मों से, किसी भी ज्ञान से, शक्ति आदि से बहुत ऊपर हैं। तपस्या आदि के प्रभाव से ऋषियों ने, सिद्धों ने ब्रह्म ज्ञान, विलक्षण शक्ति-सामर्थ्य आदि प्राप्त किया ही है, परंतु फिर भी किसी अवतार से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिये हमारी संस्कृति में इस बात को सभी समझते हैं कि भगवान् चाहे पशु शरीर में भी अवतार लेकर क्यों न आएँ तो भी किसी महान् से महान् योगी, तपस्वी या सिद्ध को उनसे तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि पशु शरीर में भी उनमें चेतना भगवान् की ही होती है। इसलिए जहाँ ईश्वर का प्रकाश होता है उसको बड़ी भारी महत्ता होती है। यहाँ तक कि भगवान् के आयुधों आदि के जो अवतार हुए हैं, उनकी भी बड़ी भारी महत्ता है और उनसे भी किन्हीं सिद्धों आदि की बराबरी नहीं की जा सकती। और जो व्यक्ति इस ईश्वर तत्त्व को जान लेता है वह शान्ति को प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार पाँचवा अध्याय 'कर्मसंन्यासयोग' समाप्त होता है।
छठा अध्याय
निर्वाण, समता एवं संसार में कर्म
श्रीभगवान् उवाच
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ १॥
१. श्रीभगवान् ने कहा : जो मनुष्य कर्म के फलों का आश्रय न लेकर करणीय कर्म को करता है, वह ही संन्यासी है और योगी है, न कि वह जो यज्ञ नहीं करता और कर्म नहीं करता।
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव ।
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ।। २।।
२. हे पाण्डुपुत्र अर्जुन ! जिसे उन्होंने संन्यास कहा है उसे वस्तुतः योग जान; क्योंकि जिसने अपने मन से कामनारूप संकल्प का परित्याग नहीं किया है ऐसा कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता।
परमात्मा स्वयं पूर्णकाम हैं। उन्हें किसी भी चीज की कोई कामना नहीं होती। इसलिये यदि व्यक्ति कामना के वशीभूत हो संकल्प करता है, कामना के वशीभूत होकर साधना करता है तो इसका अर्थ है कि वह परमात्मा के साथ युक्त नहीं है। कामना तभी होती है जब व्यक्ति अहं के साथ जुड़ा होता है, न कि अपनी सच्ची अंतरात्मा के साथ।
....श्रीगुरु बल देते हैं - और यह बहुत महत्त्वपूर्ण है - संन्यास के मूल तत्त्व के विषय में अपने बार-बार दोहराए गए दृढ़कथन पर कि यह आंतरिक संन्यास है, न कि बाह्य...। कर्म किये जाने हैं, पर किस उद्देश्य से और किस क्रम से?
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ।। ३।।
३. योग पर्वत पर आरोहण करते हुए मुनि के लिये कर्म कारण होता है; जब वह योग के शिखर पर चढ़ जाता है तो उसी मुनि के लिये आत्म-प्रभुत्व कारण होता है।
योग के शिखर पर आरोहण करते हुए पहले कर्म करने होंगेंगे, क्योंकि वहाँ कर्म 'कारण' हैं। किस चीज के कारण? आत्म-पूर्णता के, मुक्ति के, ब्रह्म-निर्वाण के कारण; क्योंकि आंतरिक संन्यास के निरंतर अभ्यास के साथ कर्म करने से यह पूर्णता, यह मुक्ति, कामनामय मन, अहंपुरुष और निम्न प्रकृति पर यह विजय सहज रूप से प्राप्त हो जाती है।
पर जब कोई शीर्ष पर पहुँच जाता है तब? तब फिर कर्म कारण नहीं रह जाते; कर्म के द्वारा प्राप्त आत्म-प्रभुत्व और धीरता अथवा आत्म-संयम की शान्ति कारण बन जाती है। परंतु पुनः, कारण किस चीज का? आत्मस्वरूप में, ब्रह्म-चेतना में स्थित बने रहने और उस पूर्ण समत्व को बनाये रखने का कारण बनती है जिसमें स्थित होकर मुक्त पुरुष के दिव्य कर्म संपन्न होते हैं।
यहाँ श्रीभगवान् स्पष्ट कर देते हैं कि संन्यास एक आंतरिक भाव है और इसका तात्पर्य कर्मों के त्याग से नहीं है। व्यक्ति को संन्यास तो कामना का करना होगा तभी आत्मप्रभुत्व स्थापित हो सकता है और तभी सच्चे रूप से कर्म किये जा सकते हैं। गीता बार-बार इसी ओर इंगित करती है कि व्यक्ति को कर्म तो करने ही होंगे क्योंकि शरीर से की जाने वाली क्रियाएँ ही कर्म नहीं होतीं अपितु मन और प्राण की क्रियाएँ भी कर्म ही होती हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से व्यक्ति कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता। योग साधना आदि में भी व्यक्ति जब किसी कामना के कारण ध्यान, चिंतन, प्राणायाम आदि करता है, फिर चाहे वह कामना कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, तो वे क्रियाएँ योग की श्रेणी में नहीं आ सकतीं। श्रीमद्भागवत् आदि ग्रंथों में हमें अनेक भक्तों की कथाओं के माध्यम से यह देखने को मिलता है कि जब भक्त किसी प्रकार के हेतु से भगवान् का चिंतन या ध्यान करता है तो बाद में भगवान् की कृपा प्राप्त करने पर उसे यह अनुभव होता है कि भगवान् के पास किसी भी निम्न हेतु से जाना तो उचित भाव नहीं है। इसलिए कर्मसंन्यास का अर्थ उस आंतरिक भाव से है जहाँ किसी कामना के कारण नहीं अपितु प्रभु को प्रसन्नता के निमित्त कर्म किये जाते हैं। इसलिए पहले ही श्लोक में भगवान् कहते हैं कि जो यज्ञ नहीं करता और कर्म नहीं करता वह न तो संन्यासी है और न योगी है।
दूसरी बात यह है कि योग के पर्वत पर आरोहण करने के लिए कर्म साधन हैं इसलिए कर्मों को करना आवश्यक है क्योंकि कर्म में मन, प्राण और शरीर की सभी क्रियाएँ समाहित हो जाती हैं। इस क्रमिक विकासमय जगत् में कर्मों के यज्ञ अर्थात् आदान-प्रदान के द्वारा ही व्यक्ति योगारूढ़ हो सकता है। परंतु जब तक व्यक्ति के भीतर कामना रहेगी तब तक वह योग नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों को यज्ञ रूप से करना आवश्यक है। यह चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं कि किस प्रकार क्रमशः व्यक्ति के यज्ञ का आरोहण होता जाता है। परंतु जब व्यक्ति आरंभ करता है तब तो उसे अपनी वर्तमान स्थिति से ही अपने यज्ञ को आरंभ करना होता है। अतः जब तक व्यक्ति किसी निश्चित स्तर तक आरोहण नहीं करता तब तक कर्म उसके साधन होते हैं जिनका त्याग नहीं किया जा सकता। और जब व्यक्ति परमात्मा के साथ युक्त हो जाता है तब उसके कर्म उन लीलामय प्रभु की लीला के अंग बन जाते हैं जिन्होंने इस संसार की रचना की है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि कर्मसंन्यास के द्वारा सामान्यतया कर्मों से निवृत्ति पाने या जंगल में चले जाने का जो अर्थ लगाया जाता है वह गीता की शिक्षा से बिल्कुल असंगत है।
मूलभूत सच्चाई और तथ्य केवल यही है कि प्रत्येक मनुष्य में प्रभु विराजमान हैं और केवल वे ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। यदि कर्मों को करते हुए व्यक्ति सचेतन होता जाता है कि उसकी इच्छाएँ, कामनाएँ आदि भी कर्म में संलग्न हैं और ऐसा नहीं होना चाहिये, तो यह भी उसकी साधना का ही एक अंग है। अभिव्यक्ति में ये चीजें रहती ही हैं, व्यक्ति अधिकाधिक सचेतन होता जाता है और वह इन चीजों पर अधिकाधिक अंकुश लगा कर आत्म-प्रभुत्व करता जाता है। इसलिए ऐसा कोई भी मनुष्य, पशु-पक्षी या ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें भगवान् की इच्छा-शक्ति अभिव्यक्त न हो रही हो। हालाँकि यहाँ गीता में जिस क्रम से विषय को समझाया गया है वह निःसंदेह बिल्कुल सही है। यह बात सच है कि मोटे तौर पर पहले तो कर्म साधना में सहायता करते हैं और फिर वे प्रभु की अभिव्यक्ति में कारण बन जाते हैं परन्तु वास्तव में तो दोनों ही चीजें साथ-साथ चलती रहती हैं। वास्तव में तो व्यक्ति विशेष के अनुसार अलग-अलग समीकरण होते हैं, इसलिए सब के लिए कोई एक नियम नहीं बनाया जा सकता। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं या हुए हैं जिनमें साधना का कोई भाव ही नहीं होता और फिर भी उनके द्वारा भगवान् की बहुत बड़ी अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिए नेपोलियन का चरित्र तो सभी जानते हैं। उसका साधना से तो दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं था। परंतु श्रीअरविन्द ने उसे भगवान् की विभूति बतलाया है जिसमें भागवत् शक्ति की क्रिया साक्षात् अभिव्यक्त हुई है। इसलिए कामनाओं, इच्छाओं आदि से भगवान् की अभिव्यक्ति रुक नहीं सकती। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये ताकि हम कोई एक सीमित मानसिक दृष्टिकोण अपना कर उससे बंध न जाएँ। मानसिक रूप से कही गई किसी भी चीज का विपर्यय भी उतना ही सही होता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में देश-काल-पात्र पर इतना अधिक बल दिया जाता था और उसी के अनुसार किसी चीज का निर्णय किया जाता था। जैसे कि, खेती आदि किसी भी कार्य को करने के लिए अलग-अलग साधनों की या औजारों की आवश्यकता होती है और कोई एक ही साधन सभी जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह बात हमें भौतिक चीजों के साथ व्यवहार में तो समझ में आती है परंतु मनोवैज्ञानिक और साधना संबंधी चीजों में हमेशा ही हम किसी एक प्रकार के सीधे-सादे नियम की माँग करते हैं। चूँकि भगवान् की अभिव्यक्ति तो एक अनंत आयामी और विराट् प्रक्रिया है जिसमें अनंत तरीके की चीजों की, प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम किसी भी बड़े से बड़े सूत्र में भी कैसे बाँध सकते हैं, यहाँ तक कि अब तक के सारे मानसिक सूत्रों को मिलाकर भी कैसे बाँध सकते हैं?
वास्तव में तो यह तामसिक वृत्ति ही है जिसके प्रभाव से व्यक्ति कहता है कि उसे तो कोई एक सीधा-सा सूत्र बता दिया जाए तो वह उसके अनुसार चलता रहे। परंतु जब परमात्मा स्वयं व्यक्ति के अन्दर विराजमान हैं तो क्या वे कभी किसी सूत्र में बंध सकते हैं? परंतु चूँकि मनुष्य सामान्यतया केवल मानसिक दृष्टिकोण से ही चीजों को देखता है इसलिए वह मन के आधार पर ही चीजों को किसी सूत्र में बाँधने का प्रयास करता रहता है। अपनी सत्ता के उच्चतर और गंभीरतर भागों के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति मन की क्रियाओं को दूर से देख सकता है, अन्यथा नहीं। मन और उसके स्वरूप के विषय में बताते हुए श्रीअरविन्द कहते हैं कि मन सत्य को जानने का यंत्र नहीं है। वह तो अधिक-से-अधिक सत्ता के निम्न भागों पर नियंत्रण करने और उच्चतर प्रेरणाओं को ग्रहण कर उन्हें क्रियान्वित करने का यंत्र है। इसलिए केवल आंतरिक तथा उच्चतर भागों से ही परमात्मा के विषय में अधिकाधिक सच्ची समझ आती है। गीता को भी यदि हम केवल सतही मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो उसकी शिक्षा में ही हमें अंतर्विरोध दिखाई देंगे और वह अलग-अलग जगहों पर अपना ही खंडन करती प्रतीत होगी। परंतु ये सभी अंतर्विरोध वास्तव में हमारी मानसिक अनम्यता के कारण होते हैं। एक व्यापक और गंभीरतर दृष्टिकोण से देखने पर ही हम गीता की शिक्षा के सच्चे अर्थ तक पहुँच सकते हैं। हालाँकि गीता के विकासक्रम का अपना एक विशिष्ट तरीका है। परंतु श्रीअरविन्द के आलोक में ये सभी चर्चाएँ पूरे विषय को अधिक स्पष्ट और समग्र रूप प्रदान करती हैं।
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ।
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।। ४।।
४. जब मनुष्य इन्द्रिय-विषयों में या फिर कर्मों में आसक्त नहीं होता, और मन में से समस्त कामनारूप संकल्प का परित्याग कर देता है तब वह मनुष्य योग के शिखर पर आरूढ़ हुआ कहा जाता है।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।। ५।।
५. 'आत्मा' के द्वारा तुम्हें आत्मा' का उद्धार करना चाहिए, तुम्हें आत्मा को (भोग या दमन के द्वारा) अधःपतित और खिन्न न होने देना चाहिए; क्योंकि आत्मा का 'आत्मा' ही मित्र है, 'आत्मा' ही शत्रु है।
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ।। ६।।
६. जिसके अंदर उच्चतर आत्मा के द्वारा निम्न आत्मा को जीत लिया गया है, उसके लिए उसका आत्मा एक मित्र है, परंतु जिसने उच्च आत्मा को प्राप्त नहीं किया है उसके लिये उसका निम्न आत्मा शत्रु के समान है और शत्रुवत् आचरण करता है।
इसमें निग्रह (अर्थात् दमन तथा बलप्रयोग) और संयम (अर्थात् उचित प्रयोग और उचित मार्गदर्शन द्वारा नियंत्रण या संयमन) ...में भेद निहित है। इनमें प्रथम, अर्थात् निग्रह संकल्प द्वारा प्रकृति पर अपनी इच्छा का तीक्ष्ण बल-प्रयोग है जो अंत में सत्ता की सहज शक्तियों को विक्षुब्ध कर देता है आत्मानमवसादयेत्; और दूसरा, अर्थात् संयम उच्चतर आत्मा द्वारा निम्नतर आत्मा को संयमित करना है जो कि सफलतापूर्वक जीव की स्वाभाविक शक्तियों को उनका उचित कर्म और उसके लिए अधिकतम कौशल प्रदान करता है, योगः कर्मसु कौशलम्...। दूसरे शब्दों में, निम्नतर आत्मा को उच्चतर आत्मा द्वारा, प्राकृत आत्मा को आध्यात्मिक आत्मा द्वारा वश में करना ही मनुष्य की पूर्णता और मुक्ति का मार्ग है।
---------------------------------------------
यहाँ कोई वास्तविक अंतर्विरोध नहीं है; ये दोनों प्रसंग ('आत्मा' के द्वारा आत्मा का vis उद्धार करो', और 'सभी धर्मों का परित्याग करो') गीता की प्रणाली में उसके योग को दो भिन्त्र XVII धाराओं को इंगित करते हैं, जिसकी उच्चतम क्रिया है पूर्ण समर्पण। व्यक्ति को सर्वप्रथम अपनी निम्नतर प्रकृति को जीतना होता है, निम्नतर क्रियाओं में उलझी हुई आत्मा को उच्चतर आत्मा की सहायता से मुक्त करना होता है जो कि इस तरह दिव्य प्रकृति में उन्नीत होती है; इसके साथ-ही-साथ व्यक्ति अपने सभी कर्मों को, योग की आंतरिक क्रिया समेत यज्ञ-रूप में पुरुषोत्तम को, परात्पर और अंतर्यामी भगवान् को अर्पित करता है। जब व्यक्ति उच्चतर आत्मा में ऊपर उठ जाता है तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह मुक्त हो जाता है, वह अन्य सभी धर्मों का परित्याग कर, एकमात्र दिव्य चेतना, दिव्य संकल्प और शक्ति तथा दिव्य आनन्द में निवास करता हुआ भगवान् के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है।
प्रश्न : उच्चतर आत्मा की सहायता से निम्नतर प्रकृति को संयमित किस प्रकार किया जाता है?
उत्तर : यदि व्यक्ति निग्रह कर के शरीर के द्वारा अमुक क्रिया को अभिव्यक्त तो नहीं होने देता परन्तु सारे दिन अपने विचारों और अपनी भावनाओं में उसके विषय में सोचता रहता है तो यह मूढ़ता है क्योंकि इससे उसके अंदर द्वंद्व पैदा हो जाएगा और उसकी सारी शक्ति ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए यदि व्यक्ति के अन्दर इच्छाशक्ति जागृत हो गई है तो उसे न केवल शारीरिक क्रियाओं को ही नियंत्रित करने में उसका उपयोग करना चाहिए अपितु उन भावनाओं और विचारों को भी वश में करने का प्रयास करना चाहिए जो कि उन क्रियाओं का मूल स्रोत हैं। हालाँकि व्यवहार में इसका अर्थ यह नहीं है कि शारीरिक क्रियाएँ चाहे जो भी क्यों न होती रहें व्यक्ति सबसे पहले उसके विषय में विचार को नियंत्रित करने का प्रयास करे। संयम का अर्थ है सबसे पहले भौतिक रूप से उन आवेगों की अभिव्यक्ति को रोकना और साथ-साथ उन विचारों, भावनाओं, आवेगों, कामनाओं आदि पर भी नियंत्रण करना जिनसे ये क्रियाएँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की बजाय यदि भौतिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए जेल में ही डालना एक समाधान हो तो आखिर हम कितने लोगों को जेल में डालेंगे? मानसिक रूप से ही हम इस विचार की असंगतता को देख सकते हैं। हमारी संस्कृति में आरंभ से ही हमारे पूर्वजों में यह अंतःप्रज्ञा विकसित थी कि यदि व्यक्ति अपनी उच्चतर आत्मा से निम्नतर आत्मा को अनुशासित करने का प्रयास करे और उसकी निम्नतर आत्मा भी इस प्रयास में उसका सहयोग करे तो वह एक मित्र है, अन्यथा तो वह एक शत्रु की भाँति ही कार्य करती है।
हमारी आंतरिक सत्ता तो सदा ही हमारी सच्ची मित्र होती है क्योंकि वह तो हमारा अपना सच्चा स्वरूप है, हम स्वयं ही हैं। जब हम अपनी उच्चतर सत्ता के द्वारा निम्नतर सत्ता को सुधारने का प्रयास करते हैं तो जब वह भी अपना सहयोग प्रदान करती है और धीरे-धीरे उसमें सुधार आता जाता है तब वह हमारी शत्रु न रहकर सहायक बन जाती है, हमारी मित्र बन जाती है। तब हम पाते हैं कि हमारी निम्न प्रकृति की वृत्तियाँ गलत नहीं हैं, वे तो केवल अपने सही स्थान पर नहीं हैं, और जब वे अपने उचित स्थान पर आ जाती हैं तो वे ही वृत्तियाँ दिव्य अभिव्यक्ति में सहायक बन जाती हैं।
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ।। ७।।
७. जब व्यक्ति ने अपने आत्मा को जीत लिया होता है और पूर्ण आत्म-प्रभुत्व एवं आत्मसंयम की शांति को प्राप्त कर लिया होता है तब उसका परम् आत्मा शीत एवं ऊष्णता में, सुख एवं दुःख में और मान एवं अपमान में अपने भीतर स्थित एवं प्रतिष्ठित रहता है।
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।। ८॥
८. जो आत्मज्ञान से तृप्त है, जो निश्चल आत्मस्थित है, जिसने अपनी इन्द्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो ढेले, पत्थर और सोने को समान समझता है, ऐसे योगी को योगयुक्त कहा जाता है।
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।। ९।।
९. जो मनुष्य सुहृद्, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु के प्रति और सत्कर्म करनेवालों और दुष्कर्म करनेवालों के प्रति समभाव रखता है, वह श्रेष्ठ होता है।
इस अध्याय के चौथे श्लोक में कहा गया है कि जब मनुष्य इन्द्रिय-विषयों में या फिर कर्मों में आसक्त नहीं होता, और मन में से समस्त कामनारूप संकल्प का परित्याग कर देता है तब वह मनुष्य योग के शिखर पर आरूढ़ हुआ कहा जाता है। यहाँ यह संकेत नहीं है कि योग के शिखर पर आरूढ़ मनुष्य कर्म नहीं करता, वह कर्म तो करता है परन्तु उनमें आसक्त नहीं होता क्योंकि वह किसी कामना के वशीभूत हो कर्मों को नहीं करता। बहुत से लोग इस श्लोक का यह अर्थ निकाल लेते हैं कि योगारूढ़ मनुष्य अपनी इन्द्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। वास्तव में जो चीज कर्मों में विकृति पैदा करती है वह है उनमें जुड़ी कामना और आसक्ति, न कि स्वयं वे कर्म। जैसे कि यदि हमारा किसी के साथ गहरा संबंध है परंतु उस संबंध के साथ गहरी आसक्ति भी है तो उस आसक्ति से बचने के लिए सामान्यतया संबंध-विच्छेद करने की सलाह दी जाती है। परंतु ऐसा करना हमारे हृदय की अभिव्यक्ति का बलपूर्वक दमन करना हुआ और इससे तो वह शुष्क हो जाएगा। इसकी बजाय हमें उस आसक्ति को दूर करना चाहिये और सच्चे रूप में, आत्मा की दृष्टि से संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये। क्योंकि परमात्मा के दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए ही तो हमारा जीवन बना है। और यदि हम किसी से संबंध रखना ही छोड़ देंगे तब तो हमें दिव्य प्रेम कैसे प्राप्त होगा और उसकी अभिव्यक्ति हम किस प्रकार कर पाएँगे। सामान्यतया जब हम किसी से संबंध बनाते हैं तो उसके माध्यम से केवल अपने-आप की तुष्टि पर ही केन्द्रित होते हैं और ऐसे संबंध में प्रेम का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसकी बजाय सच्चा तरीका है संबंध को आत्मा के आधार पर स्थापित करना। यही बात सभी चीजों पर लागू होती है। कभी-कभी मार्ग में यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ संबंधों को एकदम तोड़ दिया जाये क्योंकि आंतरिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि उनका सच्चे रूप में परिवर्तन किया जा सके।
प्रश्न : यहाँ इस श्लोक का क्या अर्थ है कि, "जब व्यक्ति ने अपने आत्मा को जीत लिया होता है और पूर्ण आत्म-प्रभुत्व एवं आत्मसंयम की शांति को प्राप्त कर लिया होता है तब उसका परम् आत्मा शीत एवं ऊष्णता में, सुख एवं दुःख में और मान एवं अपमान में अपने भीतर स्थित एवं प्रतिष्ठित रहता है"?
उत्तर : इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति के अन्दर समता आ जाती है तब वह अपनी आत्मा को जीत कर परमात्मा में समाहित हो जाता है। सामान्यतया व्यक्ति की बाहरी प्रकृति, उसके मन, प्राण और शरीर की क्रिया अहं की तुष्टि पर ही केन्द्रित होती है और उसी के दृष्टिकोण से वह अपनी इच्छाओं और कामनाओं के अनुसार कुछ चीजों का वरण करता है और कुछ को छोड़ देता है। इसलिए जीतने का अर्थ है कि व्यक्ति इस अहं-केंद्रितता को अधिकाधिक छोड़कर केवल परम् आत्मा की इच्छा पर आधारित होता जाता है और केवल उसकी इच्छा को ही पूरा करने का प्रयास करता है। तब धीरे-धीरे उसे निम्नतर प्रकार के स्पंदन आने बंद हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपनी निम्नतर प्रकृति को अनुशासित कर लेता है तब यह स्थिति स्वयं ही स्थापित हो जाती है। हालाँकि यह कर पाना आसान काम नहीं है।
आत्मा में स्थित होने के पश्चात् भी जब तक भौतिक रूपांतर सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हमारी निम्नतर प्रकृति का किसी भी समय हस्तक्षेप हो सकता है और वह अपना प्रभाव डाल सकती है और सारे संतुलन को कम या अधिक समय के लिए भंग कर सकती है, क्योंकि रूपांतर से पहले जब तक हम उच्चतर चेतना में रहते हैं तब तक तो चीजें हमारे नियंत्रण में रहती हैं परंतु उस स्थिति से नीचे आते ही हम निम्नतर प्रकृति के चंगुल में फंस सकते हैं। क्योंकि तब हममें अपनी अवचेतना से आने वाली चीजों को रोकने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती। इसलिए जब तक अवचेतना विजित नहीं हो जाती, तब तक हम कभी भी अपनी निम्नतर प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने वश में नहीं कर सकते। स्वयं श्रीरामकृष्ण जी को एक बार यह भाव उठा कि वे कामिनी-कांचन से ऊपर उठ चुके हैं परंतु जैसे ही इस विचार ने उनकी अवचेतना को स्पर्श किया वैसे ही उसमें से उसकी प्रतिक्रियास्वरूप काम का भयंकर आवेग उठा। तब उन्होंने माँ काली से प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य के अतिरिक्त सभी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि को उन्हें सौंप दिया था। इससे यह पता चलता है कि जब तक जड़-भौतिक तत्त्व तक का रूपांतरण नहीं हो जाता तब तक पूर्ण रूप से निम्नतर चीजों का निराकरण नहीं हो सकता।
आध्यात्मिक पूर्णता की प्रथम आवश्यकता है एक पूर्ण समता...। परम् दिव्य प्रकृति समता पर प्रतिष्ठित है। उसके सम्बन्ध में यह कथन सभी अवस्थाओं में सत्य है, भले हम परमोच्च सत्ता को शुद्ध एवं प्रशान्त पुरुष तथा आत्मा के रूप में देखें या विश्व-सत्ता के दिव्य स्वामी के रूप में...।
पदार्थों के स्वामी उनकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित या विक्षुब्ध नहीं हो सकते; यदि वे प्रभावित या विक्षुब्ध हो जाएँ तो वे उनके अधीन होंगे न कि स्वामी, अपने परम् स्वतंत्र संकल्प और ज्ञान के अनुसार तथा उनके सम्बन्धों के पीछे जो कुछ विद्यमान है उसके आन्तरिक सत्य और उसकी आन्तरिक आवश्यकता के अनुसार उनका विकास करने के लिये मुक्त नहीं होंगे, वरन् इसके विपरीत अस्थायी आकस्मिक संयोग और घटनाओं की माँग के अनुसार कार्य करने के लिये विवश होंगे।
...स्वामी की पूजा... माँग करती है कि हम अपने में, सब वस्तुओं तथा सभी घटनाओं में उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानें तथा हर्षपूर्वक स्वीकार करें। समत्व ही इस पूजा का लक्षण है; आत्मा की वेदी ही है जिस पर सच्चा समर्पण एवं पूजन किया जा सकता है। ईश्वर सर्वभूतों में समान रूप से हैं, हमें अपने-आप में और दूसरों में, ज्ञानी और अज्ञानी में, मित्र और शत्रु में, मनुष्य और पशु में, पापी और पुण्यात्मा में किसी प्रकार का भी तात्त्विक भेद नहीं करना चाहिये। किसी से घृणा नहीं करनी चाहिये, किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी से जुगुप्सा नहीं करनी चाहिए; क्योंकि सभी में हमें उस एकमेव के दर्शन करने हैं जो स्वेच्छापूर्वक प्रकट या प्रच्छन्न है...।
समता का अर्थ कोई कोरा अज्ञान अथवा अंधापन नहीं है, यह हमसे दृष्टि के धुँधलेपन की तथा समस्त विविधता के अन्त की माँग नहीं करती और न इसे ऐसा करने की आवश्यकता ही है। (इस समता में) भिन्नता रहती है, अभिव्यक्ति की विविधता रहती है और इस विविधता को हम भली-भाँति समझेंगे, – पहले जब हमारी दृष्टि पक्षपातपूर्ण तथा भ्रान्तिपूर्ण प्रेम और घृणा से, स्तुति और निन्दा से, सहानुभूति और वैर-विरोध से तथा राग और द्वेष से मलिन थी तब हम इसे जितना समझ पाते थे उसकी अपेक्षा अब बहुत अधिक उचित रूप में समझ पाएँगे। परन्तु इस विविधता के पीछे हम सदा उस परम् पूर्ण तथा अक्षर ब्रह्म को ही देखेंगे जो इसके अन्दर विराजमान है और किसो भी विशिष्ट अभिव्यक्ति के - चाहे वह हमारे मानवीय मानदण्डों को सुडौल एवं पूर्ण प्रतीत होती हो या बेडौल एवं अपूर्ण और चाहे वह मिथ्या एवं अशुभ ही क्यों न प्रतीत होती हो - सज्ञान प्रयोजन तथा दिव्य आवश्यकता को हम अनुभव करेंगे और जानेंगे अथवा यदि यह हमसे छिपी हुई हो तो कम-से-कम इसमें विश्वास अवश्य करेंगे... इसीलिए हम स्वामी के हाथों से सभी वस्तुओं को सम भाव के साथ ग्रहण करेंगे। जब तक दिव्य विजय का मुहूर्त नहीं आ जाता तब तक हम असफलता को भी शान्तिपूर्वक उसी प्रकार विजय को ओर जाने वाले पथ के रूप में स्वीकार करेंगे जिस प्रकार सफलता को। दारुणतम पीड़ा और दुःख कष्ट से भी, यदि दिव्य विधान में वे हमें प्राप्त हों, तो भी हमारे हृदय, मन और तन विचलित नहीं होंगे, और न ये तीव्र-से-तीव्र हर्ष एवं सुख से ही अभिभूत होंगे...।
यह समता सुदीर्घ अग्नि-परीक्षा तथा धीर आत्म-साधना के बिना नहीं आ सकती; जब तक कामना प्रबल होती है तब तक निस्तब्धता की तथा कामना की थकावट की घड़ियों को छोड़कर समता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकती, और तब (उन घड़ियों में भी) यह, सम्भवतः, सच्ची शान्ति तथा तात्त्विक आध्यात्मिक एकता होने की अपेक्षा कहीं अधिक निष्क्रिय उदासीनता, या कामना की अपने आप से झिझक ही होगी। इसके अतिरिक्त, इस साधना के या आत्मा की समता के इस विकास के अपने आवश्यक काल एवं अवस्थाएँ होती हैं। साधारणतया हमें सहिष्णुता की अवस्था से प्रारम्भ करना होता है; क्योंकि हमें सब स्पर्शों का सामना करना, उन्हें झेलना तथा आत्मसात् करना सीखना है। अपने अंदर के हर एक तंतु को हमें यह सिखाना होगा कि जो चीज दुःख देती तथा घृणा पैदा करती है उससे यह झिझके या सिकुड़े नहीं और जो वस्तु प्रिय लगती तथा आकृष्ट करती है उसकी ओर उत्सुकतापूर्वक लपके नहीं, अपितु प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करे, उसका सामना करे, उसे सहन करे तथा वश में करे। सभी स्पर्शों को सहने के लिये हमें सशक्त होना चाहिये, केवल उन्हीं को नहीं जो हमारे लिये विशिष्ट और निजी हों, वरन् उन्हें भी जो हमारे चारों ओर के तथा ऊपर या नीचे के लोकों एवं उनके निवासियों के साथ हमारी सहानुभूति या संघर्ष से हमें प्राप्त हों। अपने ऊपर होने वाली मनुष्यों, पदार्थों और शक्तियों की क्रिया को तथा अपने साथ उनके संघर्षण को, देवताओं के दबाव और असुरों के आक्रमणों को हम शान्त भाव से सहन करेंगे; अपनी आत्मा की अचल गहराइयों में हम उस सब का सामना करेंगे और उसे अपने अन्दर पूर्ण रूप से निमज्जित कर लेंगे जो कुछ आत्मा के अनन्त अनुभव के रास्ते हमारे सामने सम्भवतः आ सकता है। यह समता की तैयारी का तपस्यापूर्ण काल है, यद्यपि यह इसकी एक सर्वथा प्रारम्भिक अवस्था है तथापि यह वीरतापूर्ण काल है। परन्तु शरीर और हृदय एवं मन को इस दृढ़ सहिष्णुता को भागवत् इच्छाशक्ति के प्रति आध्यात्मिक अधीनता के स्थिर भाव का सहारा देना होगाः इस जीते-जागते पुतले को, अपनी पूर्णता को गढ़ने वाले भागवत् हस्त के स्पर्श के प्रति, दुःख में भी, नत होना होगा - कठोर व साहसपूर्ण सहमतिपूर्वक ही नहीं, अपितु ज्ञानपूर्वक अथवा उत्सर्ग के भाव में। ईश्वर-प्रेमी की ज्ञानपूर्ण, भक्तिपूर्ण अथवा यहाँ तक कि करुणापूर्ण तितिक्षा भी सम्भवनीय है और इस प्रकार की तितिक्षा उस निरी बर्बर और स्व-निर्भर सहिष्णुता से अधिक अच्छी होती है जो ईश्वर के इस आधार को अत्यन्त कठोर बना सकती है; क्योंकि इस प्रकार की तितिक्षा एक ऐसी शक्ति तैयार करती है जो ज्ञान और प्रेम को धारण कर सकती है; इसकी स्थिरता एक ऐसी गंभीरतः प्रेरित शान्ति होती है जो सहज ही आनन्द में परिणत हो जाती है। उत्सर्ग और तितिक्षा के इस काल का लाभ यह होता है कि हमें समस्त आघातों और सम्पर्कों का सामना करने वाला आत्मबल प्राप्त हो जाता है।
इसके बाद उस उच्चासीन तटस्थता एवं उदासीनता का काल आता है जिसमें आत्मा हर्ष और विषाद से मुक्त हो जाती है और सुख की लालसा के पाश से तथा दुःख-दर्द के शूलों के अँधेरे जाल से छूट जाती है। सभी वस्तुओं, व्यक्तियों और शक्तियों पर, अपने और दूसरों के सभी विचारों, भावों संवेदनों और कार्यों पर आत्मा ऊपर से अपनी दृष्टि डालती है, जो स्वयं अखण्ड एवं निर्विकार रहती है और इन चीजों से विचलित नहीं होती। यह समता की तैयारी का चिन्तनात्मक या दार्शनिक काल है, एक विशाल तथा अतिमहान् गति है। परन्तु इस उदासीनता को कर्म तथा अनुभव से निष्क्रिय पराङ्गमुखता के रूप में स्थायी नहीं हो जाना चाहिये; यह व्याकुलता, विरक्ति तथा अरुचि से उत्पन्न घृणा नहीं होनी चाहिये, न ही यह निराश या असन्तुष्ट कामना की ठिठक या उस पराजित एवं असन्तुष्ट अहं की उद्विग्नता होनी चाहिये जो अपने तीव्र या आवेशपूर्ण लक्ष्यों से बलात् पीछे हटा दिया गया है। पीछे हटने की ये चेष्टाएँ अपरिपक्व आत्मा में अवश्यमेव प्रकट होती हैं और आतुर एवं कामना-चालित प्राणिक प्रकृति को निरुत्साहित कर के ये एक प्रकार से प्रगति में सहायक भी हो सकती हैं, किन्तु ये सब वह पूर्णता नहीं हैं जिसकी ओर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस उदासीनता या तटस्थता की प्राप्ति के लिये हमें प्रयत्न करना होगा वह है वस्तुओं के स्पर्शों से परे उच्च-अवस्थित आत्मा की प्रशान्त श्रेष्ठता की; यह उन स्पर्शों को देखती तथा स्वीकार या अस्वीकार करती है, पर अस्वीकृति की अवस्था में चलायमान नहीं होती और स्वीकृति से वशीकृत नहीं हो जाती। यह अपने-आप को उस प्रशान्त आत्मा तथा आत्म-तत्त्व के निकट और उससे सम्बद्ध तथा एकमय अनुभव करने लगती है जो स्वयंभू है और प्रकृति के व्यापारों से पृथक् है, पर जो विश्व की गति और क्रिया से अतीत, शान्त एवं अचल सद्वस्तु का एक अंश रहकर या उसमें निमज्जित होकर उन व्यापारों को आश्रय देता तथा सम्भव बनाता है। उच्च अतिक्रमण के इस काल के फलस्वरूप एक ऐसी आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है जो जागतिक गति की मृदुल हिलोरों अथवा तूफानी तरंगों और लहरों से आन्दोलित और उद्वेलित नहीं होती।
इसमें मूल बात यह है कि हमें यह बोध हो जाता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब बिल्कुल ठीक हो रहा है क्योंकि उसमें हमारे भीतर की कोई चीज अभिव्यक्त हो रही है। और तब हम किन्हीं घटनाओं से विचलित नहीं होते। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति उदासीन या निवृत्तिपरक भाव अपना लेता है, अपितु इसका अर्थ यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह सब हमारे अहं अथवा मोह आदि के कारण नहीं करते अपितु परमात्मा से एक होकर उनकी लीला में अपनी भूमिका के रूप में करते हैं।
यदि हम आन्तर परिवर्तन की इन दो अवस्थाओं में से किसी में भी बद्ध या अवरुद्ध हुए बिना इन्हें पार कर सकें, तो हम उस महत्तर दिव्य समता में प्रवेश पा लेंगे जो आध्यात्मिक उत्साह तथा शान्त हर्षावेश को धारण करने में समर्थ है और जो पूर्णताप्राप्त आत्मा की एक आनन्दमयी, सर्वबोधी और सर्वसंपन्न समता है - उसकी सत्ता की एक ऐसी प्रगाढ़ तथा सम विशालता एवं परिपूर्णता है जो सब वस्तुओं को अपने में समाहित करती है। यह सर्वोच्च अवस्था है और इसे प्राप्त करने का पथ भगवान् तथा विश्वजननी के प्रति पूर्ण आत्मदान के हर्ष में से होकर जाता है। क्योंकि, तब शक्ति एक आनन्दपूर्ण प्रभुत्व से सुशोभित होती है, शान्ति गहन होकर आनन्द में परिणत हो जाती है, दिव्य शांत-स्थिरता से संपन्न स्थिति को उन्नीत कर दिव्य गति से संपन्न स्थिति का आधार बना दिया जाता है। परन्तु यदि यह महत्तर पूर्णता सिद्ध होनी है तो आत्मा की उस तटस्थ उच्चासीनता या उदासीनता को, जो पदार्थों, व्यक्तियों, गतियों और शक्तियों के निरंतर परिवर्तन या प्रवाह पर ऊपर से दृष्टिपात करती है, परिवर्तित होना होगा और दृढ़ तथा शान्त आत्मनिवेदन और सबल एवं तीव्र समर्पण के एक नये भाव में परिणत हो जाना होगा। यह आत्मनिवेदन तब ईश्वरेच्छा के प्रति निराश सहमति का नहीं, अपितु सहर्ष स्वीकृति का भाव होगाः क्योंकि तब दुःख झेलने अथवा किसी भार या सूली का कष्ट सहने का भाव तनिक भी नहीं होगा; प्रेम और आनन्द तथा आत्मदान का हर्ष ही इसका उज्ज्वल ताना-बाना होगा। यह समर्पण केवल उस दिव्य संकल्प के प्रति ही नहीं होगा जिसे हम अनुभव और स्वीकार एवं शिरोधार्य करते हैं, वरन् इस संकल्प में निहित उस दिव्य प्रज्ञा के प्रति भी होगा जिसे हम अंगीकार करते हैं और इसके अन्तर्निहित उस दिव्य प्रेम के प्रति भी जिसे हम अनुभव करते और सोल्लास वहन करते हैं, - उस आत्मा अथवा आत्मसत्ता की प्रज्ञा एवं प्रेम के प्रति होगा जो हमारी और सब की परम् आत्मा एवं आत्मसत्ता है और जिसके साथ हम मंगलमय एवं परिपूर्ण एकत्व उपलब्ध कर सकते हैं। एक एकाकी शक्ति, शान्ति एवं स्थिरता ज्ञानी की चिन्तनात्मक समता का अन्तिम शब्द है; परन्तु आत्मा अपने सर्वांगीण अनुभव में अपने-आपको इस स्व-रचित स्थिति से मुक्त कर लेती है और सनातन के अनादि और अनंत आनन्द के परम् सर्वालिंगनकारी उल्लास के सागर में प्रवेश करती है। तब हम अन्ततः सभी स्पर्शों को आनन्दपूर्ण समता से ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हम उस अविनश्वर प्रेम तथा आनन्द का संस्पर्श अनुभव करते हैं जो वस्तुओं के अन्तस्तल में सदा-सर्वदा प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है। इस वैश्विक एवं (सभी कुछ में) समान हर्षावेश के इस शिखर पर पहुँचने का परम् फल होता है आत्मा का आनन्द, असीम आनन्द के प्रथम द्वारों का उद्घाटन और एक ऐसे दिव्य हर्ष की प्राप्ति जो मन और बुद्धि से परे है।
उदासीनवत् समता आरोहण का एक सोपान है जहाँ हम इतने पर्याप्त ऊँचे उठ जाते हैं कि हमारे लिये किन्हीं भी निम्नतर चीजों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। परन्तु यह कोई बहुत उच्च स्थिति नहीं है। इस स्थिति से अलग जब हम यह महसूस करें कि सर्वत्र परमात्मा ही विद्यमान हैं और हमारा उनके साथ सतत् आनन्द नृत्य चल रहा है और संपूर्ण संसार प्रभु के आनन्द के लिये है, तो यह अवस्था ही बिल्कुल भिन्न है। हमारी चेतना में तो हम उस आनन्द की कल्पना भी नहीं कर सकते जो श्रीकृष्ण को द्रौपदी के चीर को बढ़ाने में आया होगा। इस स्थिति में तो ज्ञान, वैराग्य, समता आदि की, मन को भगवान् की ओर मोड़ने की बातों की तो कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह जाती क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा मन हमारे अपने पास तो होता ही नहीं। वह तो प्रभु को अर्पण हो चुका होता है और हम उस आनन्द नृत्य में शामिल हो जाते हैं जहाँ ज्ञान, वैराग्य, समता आदि का तो प्रवेश ही संभव नहीं है। परन्तु उस आनन्द नृत्य में कोई अकर्मण्यता नहीं होती। स्वयं भगवान् कृष्ण के जीवन को ही हम देखें कि किस प्रकार उन्होंने जन्म पूर्व से लेकर जीवनपर्यंत महान् एवं घोर कर्म किये। हमारे अपने काल में ही हम श्रीअरविन्द का एवं श्रीमाताजी का जीवन चरित देख सकते हैं जिन्होंने इतना विराट् कर्म किया जितना कि कोई कल्पना तक नहीं कर सकता।
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।। १० ।।
१०. योगी समस्त कामना और संग्रह करने की भावना को मन से निकालकर, अपने चित्त और संपूर्ण सत्ता को संयत कर के, अकेला एकान्त में बैठकर निरंतर आत्मा (परमात्मा) के साथ युक्त होने का अभ्यास करे।
परन्तु आखिरकार इस योग को प्राप्त करना कोई सुगम बात नहीं है, जैसा कि अर्जुन वास्तव में आगे चलकर सूचित करता है, क्योंकि इस चंचल मन की सदा ही बाह्य पदार्थों के आक्रमणों के द्वारा इस उच्च अवस्था से नीचे खींच लिये जाने की और पुनः शोक, आवेश और वैषम्य के जोरदार कब्जे में जा गिरने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए, मालूम होता है कि, गीता में ज्ञान और कर्म की अपनी साधारण पद्धति के साथ-साथ राजयोग की विशिष्ट ध्यान-प्रक्रिया भी बतायी गयी है जो एक शक्तिशाली अभ्यास है मन और उसकी सब वृत्तियों के पूर्ण निरोध का एक प्रबल साधन है।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ।। ११ ।।
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।
उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।। १२ ।।
११-१२. वह योगाभ्यासी मनुष्य एक पवित्र स्थान में न बहुत अधिक ऊँचे न बहुत नीचे क्रमशः मृगचर्म और वखवाले अपने दृढ़ आसन को स्थापित करे; उस आसन पर बैठ कर मन को एकाग्र कर के चित्त और इन्द्रियों को क्रियाओं को संयत कर के आत्म-शुद्धि के लिये योग का अभ्यास करे।
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ।। १३ ।।
प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ।। १४।।
१३-१४, पीठ, सिर और गर्दन को सीधे और निश्चल रखते हुए, स्थिर होकर, दृष्टि को अपनी नासिकाग्र में स्थिर कर के और इधर-उधर न देखते हुए मन से भय को दूर हटाकर, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, मन को संयत कर के, शांत चित्त होकर, मुझमें (अर्थात् भगवान् में) अपने चित्त को लगाकर, भगवत्परायण होकर, योग में स्थिर होकर बैठे।
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।। १५।।
१५. इस प्रकार अपने मन को संयत किया हुआ योगी निरंतर अपने-आपको योग में नियुक्त करता हुआ मुझमें प्रतिष्ठा वाली, निर्वाण की परमा शांति को प्राप्त होता है।
निर्वाण की यह परमा शान्ति तब प्राप्त होती है जब चित्त पूर्णतया संयत और कामनामुक्त होकर आत्मा में स्थित रहता है...फिर भी, जब तक यह शरीर है तब तक इस अवस्था का फल निर्वाण नहीं है, क्योंकि ऐसा निर्वाण संसार में कर्म करने की हर एक संभावना को, संसार के प्राणियों के साथ हर एक संबंध को दूर कर देता है। प्रथम दृष्टि में यही जान पड़ता है कि यह स्थिति निर्वाण ही होनी चाहिए। क्योंकि, जब सभी वासनाएँ और सब आवेग बन्द हो गये हों, जब मन को विचारों में प्रवृत्त होने की अनुमति ही न दी जाती हो, जब इसी मौन और एकांतिक योग का अभ्यास ही नियम हो गया हो, तब फिर और कोई कर्म करना या बाह्य संस्पर्शों और अनित्य प्रतीतियों वाले इस संसार से किसी प्रकार का संबंध रखना और अधिक संभव ही कैसे हो सकता है? निःसंदेह योगी फिर भी कुछ काल तक इस शरीर में रहता है, परंतु अब गुहा-कंदरा, वन या पर्वत-शिखर ही उसके रहने की उपयुक्ततम, और उसके दैनंदिन जीवन के एकमात्र संभव बाह्य परिवेश होंगे और सतत् समाधि आत्म-विस्मृत स्थिति ही उसका एकमात्र हर्ष और उसकी जीवनचर्या होगी। परन्तु पहली बात यह है कि गीता इस एकांतिक योग के अभ्यास काल में भी अन्य सभी कर्मों के परित्याग की सलाह नहीं देती।
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।। १६ ।।
१६. हे अर्जुन ! अवश्य ही यह योग जो न तो अत्यधिक खाता है उसके लिए है और न उसके लिए जो बिल्कुल नहीं खाता, जैसे कि यह उसके लिए भी नहीं है जो अत्यधिक सोता है और न ही उसके लिये जो जागता ही रहता है।
[तापसिक उपायों से....कोई लाभ नहीं होता। तुम केवल अपने-आपको यह धोखा देते हो कि तुमने प्रगति कर ली है, परंतु उससे लाभ कुछ नहीं होता। इसका प्रमाण यह है कि यदि तुम अपने तापसिक उपाय बन्द कर दो, तो समस्या पहले से भी अधिक प्रबल हो जाती है; और वह प्रतिशोध के भाव से पुनः लौट आती है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम किन चीजों को तापसिक उपाय कहते हो। यदि इसका अर्थ तुम्हारी सभी कामनाओं की तुष्टि में प्रवृत्त न होना हो तो यह वास्तव में तपश्चर्या नहीं, यह सामान्य बुद्धि है। यह एक भिन्न चीज है। तापसिक उपायों से तात्पर्य ऐसी चीजों से है जैसे बार-बार उपवास करना, अपने-आपको शीत सहने के लिये बाध्य करना... वस्तुतः, अपने शरीर को कुछ यंत्रणा देना। वास्तव में, यह तुम्हें मात्र आध्यात्मिक अभिमान देता है, इससे अधिक कुछ नहीं। इससे किसी चीज पर अधिकार नहीं प्राप्त होता। यह अत्यंत आसान है। लोग इसे इसलिए करते हैं क्योंकि यह बहुत सरल है, बहुत सहज है। ठीक इसलिए क्योंकि इससे अभिमान सर्वथा संतुष्ट होता है, और दर्प इससे फूल सकता है, इसलिये यह बहुत सरल हो जाता है। व्यक्ति अपने तापसिक गुणों का बड़ा प्रदर्शन करता है, और इस तरह अपने-आपको एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मान बैठता है, और इससे उसे बहुत-सी चीजें सहन करने में सहायता मिलती है।
अपने आवेगों को शांत स्थिर भाव से वश में करना और उन्हें प्रकट होने से रोकना, वह भी बिना तापसिक उपायों को अपनाये, बहुत अधिक कठिन है – बहुत अधिक! अपने पास कुछ भी न रखने की अपेक्षा जो चीजें तुम्हारे पास हैं उनके साथ आसक्त न होना बहुत अधिक कठिन है। यह बात सदियों से जानी जाती रही है। अपने अधिकार की वस्तुओं के बिना रहने या अपनी चीजों को कम-से-कम कर देने की अपेक्षा, तुम्हारे पास जो कुछ है उससे आसक्त न होने के लिए बहुत अधिक क्षमता या गुण की आवश्यकता होती है। यह बहुत अधिक कठिन है। यह नैतिक मूल्य की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ कोटि की चीज है। बस, यही मनोवृत्ति: कि जब कोई चीज तुम्हारे पास आये तो ले लेना, उसका उपयोग करना; और फिर जब किसी कारण से वह चली जाए तो उसे जाने देना और खेद न करना। जब वह आये तो मना न करना, अपने-आपको स्थिति के अनुकूल बनाना सीखना और जब वह चली जाये तो खेद न करना।
गीता का योग किन्हीं तापसिक उपायों से सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिये अगले ही श्लोक में भगवान् कह देते हैं कि "जिसका भोजन और विहार (क्रीड़ा), कर्मों में किया हुआ प्रयास, सोना और जागना सब युक्त हैं उसके लिये योग दुःख का नाश करनेवाला होता है।" श्रीमाताजी ने कहा कि अन्ततोगत्वा सभी तापसिक उपायों का एक ही परिणाम होता है और वह है आध्यात्मिक अभिमान की वृद्धि। इन साधनों के अभ्यास से साधक को यदि कोई छोटी-मोटी सिद्धि या शक्ति प्राप्त हो जाये तब फिर तो उसके अभिमान की कोई सीमा ही नहीं रहती। इसीलिए गीता ने इन किन्हीं भी उपायों पर बल न देकर सभी क्रियाओं में भगवान् के साथ युक्त होने पर ही बल दिया है।
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।। १७।।
१७. जिसका भोजन और विहार (क्रीड़ा), कर्मों में किया हुआ प्रयास, सोना और जागना सब युक्त हैं उसके लिये योग दुःख का नाश करनेवाला होता है।
प्रायः इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि यह सब परिमित, नियमित और उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए, और इसका यह आशय हो भी सकता है। परन्तु जो भी हो, जब योग प्राप्त हो चुका हो तब इन सबको एक दूसरे ही अर्थ में 'युक्त' होना चाहिए, उस अर्थ में जिसमें यह शब्द गीता के अन्य सब स्थानों में साधारण रूप से व्यवहार में लाया गया है। खाते-पीते, सोते-जागते और कर्म करते, सभी अवस्थाओं में योगी तब भगवान् के साथ 'युक्त' रहेगा और उसके द्वारा सभी कुछ भगवान् की ही चेतना में किया जाएगा, इस रूप में कि भगवान् ही उसकी आत्मा और 'सर्वमिदं' होंगे तथा वह होंगे जो उसके अपने जीवन और कर्म को आश्रय देते हैं तथा उसे धारण करते हैं। कामना, अहंकार, व्यक्तिगत संकल्प और मन के विचार केवल निम्न प्रकृति में ही कर्म के हेतु होते हैं; जब अहंकार लुप्त हो जाता है और योगी ब्रह्म हो जाता है, और यहाँ तक कि जब वह एक परात्पर चेतना और विश्व-चेतना में ही रहता और स्वयं वही बन जाता है, तब कर्म उसी में से सहज रूप से निकलता है, मानसिक विचार की अपेक्षा उच्चतर ज्योतिर्मय ज्ञान उससे निकलता है, उसी में से वह शक्ति निकलती है, जो व्यक्तिगत संकल्प से अलग और बहुत अधिक बलवती है और जो उसके लिये उसके कर्म करती है और उसके फलों को लाती है: फिर व्यक्तिगत कर्म बंद हो जाता है, सब कुछ ब्रह्म में ही ले लिया जाता और भगवान् के द्वारा धारण किया जाता है, मयि संन्यस्य कर्माणि।
ii. 30
इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में खाने, सोने आदि की क्रियाएँ नहीं करनी चाहिये अपितु संयमित तरीके से सभी कुछ करना चाहिये। परन्तु इसका गहरा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो भी कर्म करे वह भगवान् से युक्त होकर, उनसे जुड़ कर ही करे। 'योगः कर्मसु कौशलम्'। तब फिर वह जो कुछ भी करेगा उसमें परमात्मा की ही अभिव्यक्ति होगी।
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।। १८।।
१८. जिस समय समस्त चित्त पूरी तरह से संयत और समस्त काम्य पदार्थों के प्रति तृष्णारहित हो आत्मा में स्थित हो जाता है, तब उस योगी को 'युक्त' कहते हैं।
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ।। १९।।
१९. वायुरहित स्थान में रखे हुए दीपक की अविचल लौ के समान ही उस योगी का चित्त संयत या निरुद्ध होता है जो आत्मा से ऐक्य साधने अथवा युक्त होने का अभ्यास करता है।
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।। २० ।।
२०. जिस स्थिति में योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त शांत और निश्चल हो जाता है; जिस स्थिति में आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा में दर्शन किया जाता है, (जैसा इस बात को गलत रूप में लिया जाता है कि मन द्वारा अशुद्ध रूप से या आंशिक रूप से दर्शन किया जाता है और अहंकार द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वैसे नहीं, अपितु आत्मा द्वारा आत्म-बोध या आत्मानुभव किया जाता है) और जीव (योगी) संतुष्ट हो जाता है;
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।। २१ ।।
२१. जिस अवस्था में जीव (योगी) अपने उस सच्चे और चरम सुख को जानता है जो अतीन्द्रिय है जिसे बुद्धि द्वारा अनुभव किया जाता है, और जिस (अवस्था) में स्थित हो जाने पर वह अपनी सत्ता के आध्यात्मिक सत्य से विचलित नहीं होता;
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। २२।।
२२. और जिस आत्यंतिक सुख (अध्यात्म आनंद) को प्राप्त कर के योगी किसी भी दूसरे लाभ को उसकी अपेक्षा महत्तर नहीं मानता; जिसमें स्थित हो जाने पर वह मानसिक दुःख के भीषणतम आक्रमण से भी विचलित नहीं होता;
....जीव तृप्त होता और अपने वास्तविक परम् सुख को जानता है, वह अशान्त सुख नहीं जो मन और इन्द्रियों को प्राप्त है, अपितु वह आंतरिक और प्रशान्त आनन्द जिसमें वह मन की व्याकुलताओं से सुरक्षित होता है और फिर वह कभी अपनी सत्ता के आध्यात्मिक सत्य से च्युत नहीं होता। मानसिक दुःख का प्रचण्डतम आक्रमण भी उसे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि मानसिक दुःख हमारे पास बाहर से आता है, वह बाह्य स्पर्शों की ही प्रतिक्रियास्वरूप होता है, तथा यह उन लोगों का आंतरिक स्वतः-सिद्ध आनन्द है जो बाह्य स्पर्शों की चंचल मानसिक प्रतिक्रियाओं के दासत्व को अब और स्वीकार नहीं करते।
यहाँ गीता योगी की स्थिति का वर्णन करते हुए एक पूर्ण या अतिशय प्रकार का कथन करती प्रतीत होती है कि भीषणतम आक्रमण से भी योगी विचलित नहीं होता। यदि गीता के कर्मयोग के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस कथन पर ध्यान दें तब यह एक सही परिप्रेक्ष्य में समझ में आता है। जब इस मार्ग पर व्यक्ति अग्रसर होता है तब वह इस विषय में सचेतन होता है कि हमारी सक्रिय चेतना में बाहर से संवेदन आते रहते हैं। हालाँकि व्यक्ति का कोई भाग तटस्थ रूप से यह अवलोकन कर पाता है कि ये संवेदन बाहर से आ रहे हैं परंतु तो भी हमारी अवचेतन, भौतिक तथा प्राणिक प्रकृति से आक्रमण की आशंका सदा ही बनी रहती है। केवल पूर्ण रूपांतर के बाद ही व्यक्ति किसी भी प्रकार के आक्रमण की आशंका से पूर्ण रूप से निश्चिंत हो सकता है। परन्तु उससे पूर्व भी इतना तो किया ही जा सकता है कि ये निम्नतर प्रभाव हमारी बुद्धि को प्रभावित न कर पाएँ और वह लगभग अप्रभावित बनी रहे। श्रीअरविन्द के लेखों से हमें यह पता लगता है कि एक सापेक्ष समता की स्थिति, एक सापेक्ष प्रकार की पूर्णता की स्थिति प्राप्त की जा सकती है जहाँ हम अपेक्षाकृत रूप से अधिक समता की स्थिति में रह सकते हैं और निम्नतर प्रभाव अपेक्षाकृत रूप से हमें अधिक विचलित नहीं कर पाते। परंतु जब तक जड़-भौतिक चेतना पर विजय प्राप्त नहीं कर ली जाती तब तक हम इससे पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, एक निश्चित स्तर की शांति, संतुलन, सामंजस्य तथा समता की स्थिति अवश्य प्राप्त की जा सकती है। और जड़-भौतिक चेतना पर आज तक कभी पूर्ण विजय नहीं प्राप्त की सही है क्योंकि बिना अतिमानसिक चेतना के ऐसा करना संभव नहीं है।
तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।
स निश्वयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।। २३।।
२३. मन के साथ दुःख-दर्द के संबंध से इस मुक्ति को ही योग के नाम से जानना चाहिये। इस योग का चित्त में किसी भी प्रकार के अनुत्साह अथवा विषाद में डूबे बिना दृढ़तापूर्वक निरंतर अनुष्ठान करना चाहिए।
यह दुःख के साथ संबंध-विच्छेद करना है, दुःख के साथ मन के संयोग का विच्छेद करना है, दुःखसंयोगवियोगम्। इसी अविच्छेद्य आध्यात्मिक आनन्द की सुदृढ़ प्राप्ति का नाम योग, अर्थात् भगवान् से ऐक्य, है, यही लाभों में सबसे बड़ा लाभ है और यही वह धन है जिसके सामने अन्य सब संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए पूर्ण निश्चय के साथ, कठिनाई या विफलता जिस उत्साहहीनता को लाते हैं उसके अधीन हुए बिना, इस योग को तब तक किये जाना चाहिए जब तक मुक्ति न मिल जाए, जब तक कि किसी शाश्वत उपलब्धि के रूप में ब्रह्मनिर्वाण का आनन्द प्राप्त न हो जाए।
परंतु हृदय तथा मन की अधीरता और हमारी राजस प्रकृति की उत्सुक पर स्खलनशील इच्छा-शक्ति के कारण योग के विषम तथा संकीर्ण पथ पर इस श्रद्धा तथा धैर्य की प्राप्ति करना अथवा उसका अभ्यास करना कठिन होता है। मनुष्य की प्राणिक प्रकृति सदा ही अपने परिश्रम के फल के लिये तरसती है और यदि उसे ऐसा लगता है कि फल देने से इंकार किया जा रहा है या इसमें बहुत देर लगायी जा रही है तो वह आदर्श तथा नेतृत्व में विश्वास खो बैठती है। क्योंकि, उसका मन सदा ही पदार्थों की बाह्य प्रतीति के द्वारा ही निर्णय करता है, क्योंकि यह उस बौद्धिक तर्क की पहली सबसे भारी गहराई तक जमी हुई आदत है जिसमें वह इतने अतिशय रूप से विश्वास करता है। जब हम चिरकाल तक कष्ट भोगते या अन्धेरे में ठोकरें खाते हैं तब अपने हृदयों में भगवान् को कोसने से अथवा जो आदर्श हमने अपने सामने रखा है उसे त्याग देने से अधिक आसान हमारे लिये और कुछ नहीं होता। क्योंकि, हम कहते हैं, "मैंने सर्वोच्च सत्ता पर विश्वास किया है और मेरे साथ विश्वासघात कर के मुझे दुःख, पाप और भ्रान्ति के गर्त में गिरा दिया गया है।" या फिर, "मैंने एक ऐसे विचार पर अपने सारे जीवन की बाजी लगा दी है जिसे अनुभव के दृढ़-तथ्य खंडित तथा निरुत्साहित करते हैं। बेहतर होता कि मैं भी दूसरे उन सब के जैसा ही होता जो अपनी सीमाएँ स्वीकार करते हैं और सामान्य अनुभव के स्थिर आधार पर विचरण करते हैं।" ऐसी घड़ियों में - और कभी-कभी ये बारम्बार आती हैं और दीर्घकालिक होती हैं - समस्त उच्चतर अनुभव विस्मृत हो जाता है और हृदय अपनी कटुता में डूब जाता, उसी पर केंद्रित हो जाता है। इन्हीं अंधकारमय कालों में यह आशंका रहती है कि हम सदा के लिये पतित हो सकते हैं अथवा दिव्य कार्य या श्रम से पराङ्गमुख हो सकते हैं।
साधना पथ में आने पर भी मनुष्य के प्राण को उसकी क्रियाओं का प्रतिफल नहीं मिलता तो वह अधीर हो जाता है, विचलित हो जाता है। यदि उसे स्थूल प्रतिफल की चाह न भी हो तो भी अधिकांशतः आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने की चाह बनी रहती है, योग में सिद्धि की चाह बनी रहती है। और गहन प्रयास के बाद भी जब प्राण की ये तृष्णाएँ पूरी नहीं होतीं तो वह अधीर हो उठता है और नकारात्मक संवेदन और सुझाव भेजने लगता है जैसे कि 'यद्यपि साधना में लगे हमें एक लंबा समय बीत गया है परंतु अभी तक कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई' अथवा यह कि 'हम तो दूसरों से किसी भी भाँति कम नहीं हैं फिर भी हमें कोई उपलब्धि नहीं हुई' आदि-आदि। ये सब बहुत ही आम सुझाव हैं जो अधिकांश साधकों को साधना के किसी-न-किसी पड़ाव पर आते ही हैं। और स्थिति तब और भी भयंकर बन जाती है जब हमारी बुद्धि भी प्राण का समर्थन करने लगती है। साधना पथ पर ऐसा कौन है जिसके ये काल न आते हों। परन्तु वास्तव में यदि आत्मा ने निर्णय कर लिया है तो गिरने के बाद भी वह पुनः व्यक्ति को उसी पथ पर ले आयेगी। इसलिये गीता कहती है कि साधना के पथ पर अनवरत लगे रहो। जब तक कोई भी कामना शेष है तब तक इस प्रकार के काल आयेंगे ही। इसीलिये श्रीअरविन्द कहते हैं कि योग केवल और अनन्य रूप से भगवान् के लिये ही होना चाहिये। जब हम किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिये योग कर ही नहीं रहे होते तो फिर उसके मिलने या ना मिलने से तो हमें कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता।
परन्तु यदि कोई पथ पर दूर तक तथा दृढ़ता से चल चुका हो तो हृदय की श्रद्धा उग्र-से-उग्र विरोधी दबाव में भी स्थिर बनी रहेगी; आच्छादित या बाहर से देखने में पराजित होने पर भी, यह पहला अवसर पाते ही फिर उभर आयेगी। कारण, हृदय या बुद्धि से उच्चतर कोई चीज इसे अति निकृष्ट पतनों के होते हुए भी तथा अत्यन्त दीर्घकालीन विफलता में भी सहारा देगी। परन्तु ऐसी दुर्बलताएँ या अन्धकार की अवस्थाएँ एक अनुभवी साधक तक की प्रगति में भी गतिरोध लाती हैं और नौसिखिये के लिये तो ये अत्यन्त हो असुरक्षित या खतरनाक होती हैं। अतएव, आरम्भ से ही आवश्यक होता है कि इस पथ की विकट कठिनाई को समझा और इसे अंगीकार किया जाए और उस श्रद्धा की आवश्यकता को अनुभव किया जाए जो बुद्धि को भले हो अन्धी प्रतीत होती हो फिर भी हमारी तर्कशील बुद्धि से अधिक ज्ञानपूर्ण होती है। क्योंकि यह श्रद्धा ऊपर से मिलने वाला अवलंब है; यह उस गुप्त ज्योति की उज्ज्वल छाया है जो बुद्धि और इसके ज्ञात तथ्यों से अतीत है; यह उस निगूढ़ ज्ञान का सारभूत तत्त्व है जो प्रत्यक्ष प्रतीतियों का दास नहीं है। हमारी श्रद्धा, अटल या दृढ़ रहकर, अपने कर्मों में युक्तियुक्त या उचित सिद्ध होगी और अन्त में दिव्य ज्ञान के आत्म-प्रकटन में उन्नीत तथा रूपान्तरित हो जाएगी। सदा ही हमें गीता के इस आदेश का दृढ़ता से अनुसरण करना होगा कि "निराशा अथवा अवसाद से रहित हृदय के द्वारा योग का निरन्तर अभ्यास करना चाहिये।" सदा ही हमें संशयशील बुद्धि के समक्ष ईश्वर की यह प्रतिज्ञा दुहरानी होगी, "मैं निश्चय ही तुझे समस्त पाप एवं अशुभ से मुक्त कर दूंगा; शोक मत कर।" अन्त में, श्रद्धा की अस्थिरताएँ दूर हो जाएँगी, क्योंकि हम भगवान् की मुखछवि निहार लेंगे और भागवत् उपस्थिति को सदा ही अनुभव करेंगे। बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है कि एक बार जब हमने योग मार्ग पर
यह कदम रख दिया तब चाहे हजार जन्म भी क्यों न लग जायें, हमें इधर-उधर नहीं देखना है। किसी भी प्रकार के अन्य संवेदनों के प्रति हमें अपने आप को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। जब तक हम प्राण के कुतकों को सुनते रहेंगे तब तक आत्मा को अपनी वाणी सुनाने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिये हमें निश्चय करना होगा कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए पर हम किसी अन्य विषय के बारे में नहीं सोचेंगे। तब जाकर द्वार खुल जाते हैं। प्राण को जब तक इसकी संभावना लगेगी कि हम पथ से च्युत हो सकते हैं तब तक वह प्रयास करता रहेगा। जहाँ हमारी कमजोरी होगी प्राण वहीं आक्रमण करेगा। जब तक हममें कोई भी कमजोरी रहेगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। यह हमारी सारी कमजोरियों से हमें ऊपर उठायेगा। जब हम हमारी श्रद्धा में अडिग होंगे तब वह हमें अकेला छोड़ देगा। गीता कहती है कि जब हम बिना इधर-उधर देखे चलते रहेंगे तो हमें भागवत् द्वारों की कुंजी मिल जायेगी। परंतु अब भी हमारा ध्यान भगवान् के ऊपर केंद्रित होना चाहिये न कि इस बात पर कि साधना के द्वारा द्वार खुल जाएँगे, वह हमारा विषय नहीं है।
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।। २४।।
शनैः शनैरुपरमेद्बुद्धया घृतिगृहीतया ।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ।। २५॥
२४-२५. संकल्प से उत्पन्न होनेवाली संपूर्ण कामनाओं का निःशेष रूप से परित्याग कर के, मन के द्वारा समस्त इन्द्रियों को सब ओर से ही निवृत्त कर के (जिससे कि वे इधर-उधर न दौड़ सकें) स्थिरता से संयत बुद्धि (स्थिरबुद्धि) के द्वारा धीरे-धीरे मन की क्रिया को बंद कर देना चाहिए, मन को उच्च आत्मा में स्थिर कर के किसी भी पदार्थ के बारे में न सोचना चाहिए।
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ।। २६।।
२६. चंचल और अस्थिर मन (जब-जब और) जिस-जिस विषय की ओर बाहर जाने की चेष्टा करे (तब-तब और) वहीं-वहीं से इसे रोककर (हटाकर) आत्मा के ही वश में ले आये (आत्मा में स्थिर करे)।
प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ।। २७।।
२७. जब मन को पूरी तरह शांत कर दिया जाता है तब निश्चय ही योगी को उस आत्मा का, जो ब्रह्म बन गई है, असंवेगशील, निर्मल, उच्चतम आनन्द प्राप्त होता है।
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ।। २८।।
२८. इस प्रकार (काम-क्रोधादि) विकारों से मुक्त और सर्वदा अपने-आपको योग में नियुक्त करता हुआ योगी सरलता से और प्रसन्नता के साथ ब्रह्म के स्पर्शरूप चरम कोटि के आनन्द (परमानंद) का अनुभव करता है।
यहाँ प्रधान बल भावनामय मन, कामनामय मन और इन्द्रियों के निरोध पर दिया गया है, क्योंकि ये बाह्य स्पर्शों को ग्रहण करते हैं और हमारी सामान्य अभ्यस्त भावावेगमय प्रतिक्रियाओं के द्वारा उनका प्रत्युत्तर देते हैं; परन्तु यहाँ तक कि मानसिक विचार को भी स्वतः-विद्यमान सत्ता की शान्ति में ले जाकर स्थिर करना होगा। पहले, कामनामय संकल्प से जनित सभी कामनाओं को बिना किसी को छोड़े या बचाए निःशेष रूप से पूरी तरह से त्याग देना होगा और मन के द्वारा इन्द्रियों को वश में करना होगा ताकि वे अपनी हमेशा की अव्यवस्थित और चंचल आदत के कारण चारों ओर दौड़ती न फिरें; परन्तु इसके बाद स्वयं मन को ही बुद्धि से पकड़कर अंतर्मुख करना होगा। व्यक्ति को निश्चल बुद्धि के द्वारा मानसिक कर्म करना धीरे-धीरे बन्द कर देना चाहिए और मन को आत्मा में स्थित कर के किसी बारे में कुछ भी न सोचना चाहिए। जब-जब चंचल अस्थिर मन निकल भागे तब-तब उसका नियमन कर के उसे पकड़कर आत्मा के अधीन लाना होगा। जब मन पूर्ण रूप से शान्त हो जाए तो योगी आसानी से व प्रसन्नता से ब्रह्म के स्पर्श को, जो कि अतिशय आनन्ददायी है, अनुभव करता है।
अब प्रश्न यह उठता है कि इसे किया कैसे जाये? क्योंकि जिस प्रक्रिया का यहाँ वर्णन है उसे यदि कोई व्यवहार में लाने का प्रयास करेगा तो कुछ ही समय में वह क्लांत हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिये तो यह रास्ता बड़ा ही दुःखदायी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आन्तरिक संतुलन इस प्रकार का होता है कि उनमें त्याग और वैराग्य की भावना अधिक होती है। वे लोग किसी निर्जन स्थान पर जाकर और अत्यधिक प्रयास कर के, अनेक अभ्यास कर के मन को बहुत हद तक शांत कर लेते हैं। ऐसे लोग किसी निर्जन स्थान पर जाकर वर्षों तक कठोर साधना करते हैं। किसी एक मंत्र अथवा किसी एक ही विचार पर स्वयं को केन्द्रित कर के वर्षों तक लगे रहते हैं। बौद्ध धर्म आदि में इस प्रकार की बहुत सी पद्धतियाँ वर्णित हैं। इन पद्धतियों का अभ्यास मन के यांत्रिक स्वभाव से भी अधिक यांत्रिक रूप से किया जाता है। और इस प्रकार के निषेध के कारण मन और चित्तवृत्तियाँ स्वयं ही धीरे-धीरे शांत हो जाती हैं। जब व्यक्ति को उस अवस्था में रस आने लगता है तब वह न्यूनतम आवश्यक दैनिक कार्यों के अलावा केवल ध्यान में ही रमे रहता है। इस स्थिति को प्राप्त करना संभव है और बहुत से व्यक्तियों ने इसे प्राप्त भी किया है परन्तु हर एक की प्रकृति के लिये यह अनुकूल नहीं है। कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं को इन्द्रियों के भोगों से, संवेदनों से हठपूर्वक पूर्णतः वंचित कर देता है और ऐसा करने से चित्त की वृत्तियाँ धीरे-धीरे शांत हो जाती हैं जिससे कि अक्षर की स्थिति का अनुभव प्राप्त हो जाता है।
परन्तु इस प्रक्रिया को हम मन पर प्रभुत्व होना नहीं कह सकते क्योंकि यह तो किसी पद्धति के सहारे प्राप्त किया गया एक नियंत्रण है और जैसे ही साधक का अपने मन पर से थोड़ा-सा भी नियंत्रण कमजोर पड़ता है वह पुनः नीचे गिर जाता है। और पुनः वहाँ तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को दुबारा उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। परंतु परमात्मा तक पहुँचने के हजारों रास्तों में से यह भी एक रास्ता हो सकता है जो किसी व्यक्ति विशेष की प्रकृति के अनुकूल हो। साधना में किसी बिन्दु पर यह प्रक्रिया आवश्यक हो सकती है जो व्यक्ति को कुछ अनुभव प्रदान कर दे। इसी तरह प्राणायाम भी व्यक्ति को कुछ अनुभव प्रदान कर सकता है। और हो सकता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। परन्तु इससे व्यक्ति की प्रकृति में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार की किसी भी साधना से प्रकृति पर वह प्रभुत्व प्राप्त नहीं हो सकता जैसा भगवान् श्रीकृष्ण का कुरुक्षेत्र की भूमि पर हमें देखने को मिलता है जो कि घोर युद्ध समक्ष होने पर भी हँसते हुए गीता का उपदेश दे रहे हैं। जहाँ अर्जुन इस पूरे दृश्य को देखकर विचलित हो रहा है वहीं श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए ज्ञान दे रहे हैं। यह तो एक अद्भुत भाव है जो सामान्य बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकता।
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। २९।।
२९. जिसका आत्मा योग में युक्त हो गया है ऐसा सबको समान दृष्टि से देखनेवाला योगी आत्मा को समस्त भूतों में देखता है और समस्त भूतों को आत्मा में देखता है।
यह आत्मा ही हमारी स्वतः विद्यमान सत्ता है। यह हमारे वैयक्तिक अस्तित्व से सीमित नहीं है। यह सभी भूतों में समान, व्यापक, सबके लिए सम, अपनी अनन्तता से अखिल विश्वकर्म को धारण करनेवाली है, परंतु जो कुछ भी सीमित है उससे यह सीमित नहीं होती, प्रकृति और व्यक्तित्व के परिवर्तनों से परिवर्तित होनेवाली नहीं है। जब यह आत्मा हमारे अंदर प्रकाशित होती है, जब हम इसकी शान्ति और नीरवता का अनुभव करते हैं, तब हम इसमें संवर्द्धित हो सकते हैं; हमारा अंतःपुरुष जो अभी प्रकृति में निमज्जित होकर निम्नतर अवस्था में है उसे आत्मा में पुनः प्रतिष्ठित कर सकते हैं। हम यह उन वस्तुओं की शक्ति से कर सकते हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं - स्थिरता, समता, निर्विकार नैयक्तिकता। क्योंकि ज्यों-ज्यों हम इन चीजों में विकसित होते हैं, उन्हें अपनी परिपूर्णता तक पहुँचाते हैं और अपनी सारी प्रकृति को इनके अधीन कर देते हैं, त्यों-त्यों हम इस शांत-स्थिर, सम, निर्विकार, नैर्व्यक्तिक, सर्वव्यापक आत्मा के स्वरूप में विकसित होते जाते हैं। हमारी इन्द्रियाँ उसी नीरवता में जा पहुँचती हैं और जगत् के स्पर्शों को परम् शान्ति के साथ ग्रहण करती हैं; हमारा मन उसी नीरवता को प्राप्त हो जाता है और शान्त वैश्विक साक्षी बन जाता है; और हमारा अहंकार इसी नैयक्तिक सत्ता में विलीन हो जाता है। तब हम सभी चीजें उसी आत्मा में देखते हैं जो हम स्वयं अपने आप में बन चुके हैं; और इस आत्मा को हम सबके अन्दर देखते हैं, हम सब भूतों के साथ उनकी आत्मसत्ता में एकीभूत हो जाते हैं। इस अहंभावशून्य अथवा निष्काम शान्ति और नैयक्तिकता में रहते हुए हम जो कर्म करते हैं वे हमारे कर्म नहीं रह जाते, वे अब अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें किसी भी प्रकार से न तो बाँध सकते हैं न कोई पीड़ा ही पहुँचा सकते हैं।
परन्तु यदि वह लेशमात्र भी क्षर की क्षरशीलता में रहे तो क्या उसका इस कठिन योग के समस्त फलों को खो देने का, आत्मा को खो देने का और फिर से मन के अन्दर जा गिरने का खतरा नहीं है, भगवान् का उसे खो देने का और उसका जगत् में रम जाने का, उसका भगवान् को खो देने का और उनकी जगह फिर से अहंकार को तथा निम्न प्रकृति को पाने का खतरा नहीं है? गीता उत्तर देती है, नहीं...
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।। ३० ।।
३०. जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब को मुझ में देखता है, उसके लिये मैं खोया नहीं जाता और न ही वह मेरे लिये खोया जाता है।
क्योंकि निर्वाण की यह परम् शान्ति यद्यपि अक्षर से प्राप्त होती है, परंतु पुरुषोत्तम की सत्ता पर ही प्रतिष्ठित है, मत्संस्थाम्, और यह सत्ता व्यापक है: भगवान्, ब्रह्म, प्राणियों के इस जगत् में भी व्याप्त हैं और यद्यपि वे इस जगत् से परे हैं, किन्तु वे अपनी परात्परता में सीमित नहीं हैं। मनुष्य को सब कुछ भगवान् के रूप में देखना होगा और पूर्ण रूप से इसी दृष्टि या भाव में जोना और कर्म करना होगा; यही योग का परम् फल है।
vi.1.5
पर कर्म क्यों करें? क्या यह अधिक निरापद नहीं है कि हम स्वयं एकान्त में बैठकर इच्छा हो तो जगत् की ओर एक निगाह देख लें, उसे ब्रह्म में, भगवान् में देखें पर उसमें कोई भाग न लें, उसमें विचरण न करें, उसमें रहें नहीं, उसमें कर्म न करें और साधारणतया अपनी आंतरिक समाधि में ही रहें? क्या इस उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था का यही धर्म, यही विधान, यहो नियम नहीं होना चाहिए? गीता फिर कहती है कि नहीं: मुक्त योगी के लिए इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विधान, नियम, धर्म नहीं होता कि वह भगवान् में रहे, भगवान् से प्रेम करे और सब प्राणियों के साथ एक हो जाए, उसका जो स्वातंत्र्य है वह निरपेक्ष है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं, वह स्वयंभू है, किसी आचार, धर्म या मर्यादा से बँधा नहीं। उसे अब और अधिक योग की किसी प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब वह सतत् योग में प्रतिष्ठित होता है।
वे जो दो श्लोक हैं (२९-३०) वे हमें पुनः गीता के योग की धारा में ले आते हैं। पहली चीज है आत्मा को समस्त भूतों में देखना और समस्त भूतों को आत्मा में देखना और दूसरी है सर्वत्र परमात्मा को देखना और सब कुछ परमात्मा में देखना। और जो इस प्रकार देख लेता है वह फिर गिरता नहीं है। उसकी स्थिति स्थिर है। शुरू में जो स्थिति होती है उसमें तो हमें स्वयं को उस स्तर पर बनाये रखने का प्रयास करना पड़ता है परन्तु यदि एक बार यह अनुभव हो जाए कि हम आत्मा को, जो कि हमारी स्वतः-विद्यमान सत्ता है और हमारे वैयक्तिक अस्तित्व से सीमित नहीं है, समस्त भूतों में देख सकें और समस्त भूतों को आत्मा में देख सकें तब फिर एक सुदृढ़ स्थिति प्रतिष्ठित हो जाती है। और उसके बाद जब हम केवल परमात्मा को ही सर्वत्र देख सकें और सबमें केवल परमात्मा को ही देख सकें तब फिर अहंकार तथा निम्न प्रकृति में जा गिरने का खतरा नहीं रहता।
अब श्रीअरविन्द यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि हमने एक बार यह सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर लिया फिर हमें कर्म की क्या आवश्यकता है? गीता अगले श्लोक में कहती है, "जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर समस्त भूतों में मुझसे प्रेम करता है वह योगी चाहे जिस प्रकार रहे और कर्म करे मुझमें ही रहता और कर्म करता है।" परंतु इस स्थिति के लिए शर्त यह है कि योगी सभी भूतों में भगवान् से ही प्रेम करे। सब भूतों में केवल परमात्मा को ही देखना और फिर केवल उन्हीं से प्रेम करना तो समाधि में बैठ कर परमात्मा का ध्यान करने से तो बहुत ही परे की स्थिति है और बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। गीता कहती है कि इस स्तर को प्राप्त करने के बाद फिर योगी कुछ भी कर्म करे और कैसे भी कर्म करे वह परमात्मा में ही निवास करता है। यहाँ गीता कर्म का एक सच्चा विधान बता रही है कि किस प्रकार बिना गिरने की आशंका के सच्चे रूप से कर्म किये जा सकते हैं। क्योंकि यदि इस स्थिति का वर्णन न किया जाता और केवल वन में जाकर मन आदि को इंद्रिय विषयों से हटाकर अक्षर की शांति में जाना ही उद्देश्य होता तब तो अर्जुन इस समाधान के लिए पहले से ही इच्छुक था। परंतु तब तो गीता की सारी शिक्षा ही निरर्थक हो जाती और वह स्वयं अपनी ही बात का खंडन कर रही होती। परंतु जब योगी भगवान् को ही सब में देखता और प्रेम करता है, तब वह घोर से घोर कर्म करने पर भी अपनी स्थिति से गिरता नहीं। और यही कर्मयोग का सच्चा उपाय है। परंतु इसके बाद अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठना तो स्वाभाविक ही है कि जिस स्थिति की भगवान् चर्चा कर रहे हैं उससे पूर्व की स्थिति उसने अनुभव नहीं की है। इसीलिये वह कहता है कि "मन के चंचल होने के कारण इस योग की मैं (अपने भीतर) दृढ़ स्थिति को नहीं देखता हूँ।"
साथ ही, यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि सबमें परमात्मा दिखाई देने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को विविधता दिखना बंद हो जाती है और उसे किसी हाथी और महावत के बीच का भेद ही दिखाई नहीं देता। सबमें परमात्मा दिखना तो एक बहुत गहरा अनुभव है जिसे किसी भी मानसिक चित्रण में नहीं बाँधा जा सकता। व्यवहार में तो भगवान् स्वयं ही किन्हीं दो व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। किसी को वे प्रेम करते हैं और किसी का संहार करते हैं। परंतु दोनों ही हालतों में उनके भाव में अंतर नहीं आता। संहार कर्म भी उनके प्रेम और उनकी कृपा की ही अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए हम अपने पुराणों में सभी जगह वर्णन पाते हैं कि भगवान् दुष्टों को मारकर उनका उद्धार करते हैं और उनमें से कुछ को तो ऐसी सद्गति प्रदान करते हैं जैसी योगियों को भी दुर्लभ है। स्वयं श्रीमाँ और श्रीअरविन्द के योग-संबंधी पत्रों से हम देख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी दो साधकों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया। सभी को सुविधाएँ भी अलग-अलग प्रदान की जाती थीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें सभी के भीतर परमात्मा न नजर आते हों। परंतु वे हमारे इस तुच्छ मानसिक उपकरण की सहायता से निर्णय नहीं करते थे। इसी कारण सबके साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार करने पर भी हर एक को ऐसा महसूस होता था कि उससे श्रीमाँ अतिशय प्रेम करती हैं और वे कभी उनके निर्णयों पर संदेह नहीं करते थे क्योंकि सभी यह जानते थे कि श्रीमाँ वही करेंगी जो उसकी आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा।
इसलिए जब व्यक्ति सभी में परमात्मा के दर्शन करने लगता है तो जीवन की बहुत सी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। क्योंकि तब सभी चीजों में प्रभु की क्रिया दिखाई देने लगती है। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि इस अनुभव से कोई भौतिक रूपांतरण नहीं होता। इससे कोई अतिमानसिक रूपांतर साधित नहीं हो जाता। हाँ, इस अनुभव के बाद साधक एक स्थिति विशेष से च्युत नहीं होता। अवश्य ही पूर्ण रूपांतर साधित होने से पहले अवचेतन में से निम्न वृत्तियाँ तो उठ ही सकती हैं परंतु साधक उनसे थोड़े-बहुत काल के लिए प्रभावित होकर पुनः अपनी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है। स्थायी रूप से उस पर ये अपना प्रभाव नहीं डाल सकतीं।
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।। ३१ ।।
३१. जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर समस्त भूतों में मुझसे प्रेम करता है वह योगी चाहे जिस प्रकार रहे और कर्म करे मुझ' में ही रहता और कर्म करता है।
संसार-प्रेम तब आध्यात्मिकृत होकर, इन्द्रिय अनुभव से आत्मा के अनुभव में परिणत होकर, ईश्वर-प्रेम पर प्रतिष्ठित हो जाता है और तब उस प्रेम में कोई भय, कोई दोष नहीं रहता। निम्न प्रकृति से पीछे हटने के लिए संसार से भय और जुगुप्सा प्रायः आवश्यक हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में यह हमारे अपने अहं का भय और जुगुप्सा है जो अपने-आप को जगत् में प्रतिबिंबित करता है। परन्तु ईश्वर को जगत् में देखना सभी कुछ से निर्भय हो जाना है, यह सभी कुछ का ईश्वर की सत्ता में आलिंगन करना है; सब कुछ भगवद्रूप में देखने का अर्थ है किसी पदार्थ को नापसन्द या किसी से भी घृणा न करना, अपितु जगत् में भगवान् से और भगवान् में जगत् से प्रेम करना...
गीता सदा की ही भाँति यहाँ भी भक्ति को योग की पराकाष्ठा के रूप में ले आती है, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः; इसी को गीता की शिक्षा के लगभग संपूर्ण सार का सर्वस्व कहा जा सकता है - जो कोई सबमें स्थित भगवान् से प्रेम करता है और जिसकी आत्मा भगवदैक्य में प्रतिष्ठित है, वह चाहे कैसे भी रहता और कर्म करता हो, भगवान् में ही रहता और कर्म करता है।
भगवान् के साथ एकत्व, सब प्राणियों के साथ एकत्व, सर्वत्र सनातन भागवत् एकता की अनुभूति और इसी एकता की ओर मनुष्यों को आगे बढ़ा ले जाना ही उस जीवन का धर्म है जो गीता के उपदेशों से उत्पन्न होता है। इससे अधिक महान्, अधिक व्यापक, अधिक गंभीर और कोई धर्म नहीं हो सकता। स्वयं मुक्त होकर इस एकत्व में रहना और मानव जाति को इसी रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायता करना तथा अपने सब कर्मों को भगवान् के लिए करते हुए (कृत्स्नकर्मकृत्) और मनुष्यों को जिसका जो कर्तव्य कर्म है उसे हर्ष और उत्साह के साथ करने में बढ़ावा देना (सर्वकर्माणि जोषयन्), इससे अधिक महान् और उदार दिव्य-कर्म-विधान नहीं दिया जा सकता। यह मुक्तावस्था और यह एकत्व हमारी मानव-प्रकृति का गुप्त लक्ष्य है और यही मानव-जाति के अस्तित्व में अंतर्निहित चरम इच्छा है। इसी की ओर मनुष्यजाति को उस सुख की प्राप्ति के लिए मुड़ना होगा जिसे वह अभी तक असफल रूप से खोज रही है, ऐसा तब होगा जब मनुष्य अपने नेत्रों और अपने हृदयों को ऊपर उठाकर अपने में और अपने चारों ओर, सब भूतों में, सर्वेषु, और सर्वत्र, भगवान् को देखने लगेंगे और यह जान लेंगे कि हम सब भगवान् में ही रहते हैं और हमारी यह भेदजनक निम्न प्रकृति केवल एक कैदखाने की दीवार है जिसे तोड़ डालना होगा, या फिर अधिक-से-अधिक यह बच्चों के पढ़ने की एक पाठशाला है जिसकी पढ़ाई समाप्त कर के आगे बढ़ना होगा जिससे हम प्रकृति में प्रौढ़ और आत्मा में मुक्त हो जाएँ। ऊर्ध्वस्थित भगवान् के साथ, मनुष्य में और जगत् में स्थित भगवान् के साथ एकात्मभाव को प्राप्त होना हो मुक्ति का अभिप्राय और संसिद्धि का रहस्य है।
-----------------------------------------
ईश्वर और जगत्-विषयक आध्यात्मिक दृष्टि केवल विचारात्मक ही नहीं है, न प्रधानतः या प्रथमतः ही विचारात्मक है। वह तो प्रत्यक्ष अनुभव है और उतना ही वास्तविक, जीवंत, निकट, सतत्, प्रभावकारी तथा अंतरंग होता है जितना कि मन के लिए आकारों, पदार्थों और व्यक्तियों का इन्द्रियों द्वारा अवलोकन करना व संवेदन करना। केवल स्थूल मन ही है जो ईश्वर एवं आत्मा को कपोल कल्पना मात्र मानता है जिसे वह दृष्टिगोचर नहीं कर सकता या न ही जिसका स्वयं के सम्मुख शब्दों, नामों, प्रतीकात्मक रूपों तथा कल्पनाओं के बिना निरूपण ही कर सकता है। आत्मा आत्मा को देखती है, दिव्यीकृत चेतना भगवान् को वैसे ही प्रत्यक्ष रूप में तथा उससे भी अधिक प्रत्यक्ष रूप में, वैसे ही घनिष्ठ रूप से तथा उससे भी अधिक घनिष्ठ रूप से देखती है जितना कि शारीरिक चेतना जड़ पदार्थ को देखती है। वह भगवान् को देखती, अनुभव करती, उनका चिंतन करती तथा उनका इंद्रियानुभव करती है। क्योंकि, आध्यात्मिक चेतना को समस्त व्यक्त जगत् आत्मा के जगत् के रूप में दृश्यमान होता है तथा जड़तत्त्व का जगत् नहीं, प्राण का जगत् नहीं, यहाँ तक कि मन के जगत् के रूप में भी नहीं; ये अन्य चीजें उसकी दृष्टि में केवल ईश्वर-विचार ईश्वर-शक्ति, ईश्वर-रूप ही होती हैं। वासुदेव में निवास करने तथा कर्म करने, 'मयि वर्तते से गीता का यही तात्पर्य है। आध्यात्मिक चेतना परमेश्वर के बारे में उस घनिष्ठ तादात्म्य-ज्ञान के द्वारा सचेतन है जो चिंत्य वस्तु के किसी भी मानसिक बोध या गोचर पदार्थ के किसी भी ऐंद्रिय अनुभव से बहुत अधिक वास्तविक है।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।। ३२ ।।
३२. हे अर्जुना जो मनुष्य चाहे सुख हो अथवा दुःख, सभी कुछ को समत्व भाव से आत्मा के स्वरूप में देखता है, उसे मैं परम योगी मानता हूँ।
और इसका यह अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि स्वयं योगी, दूसरों के दुःख में ही क्यों न हो, अपने दुःख रहित आत्मानन्द से गिर जायेगा और पुनः सांसारिक दुःख अनुभव करने लगेगा, अपितु यह कि दूसरों में उन द्वन्द्वों के खेल को देखकर, जिन्हें छोड़कर वह स्वयं ऊपर उठ चुका है, वह सब कुछ आत्मवत् और सबमें अपनी आत्मा को, सबमें ईश्वर को देखेगा और इन चीजों के बाह्य रूपों में क्षुब्ध या मुग्ध न होकर केवल उनकी सहायता करने और उनका दुःख दूर करने के भाव से प्रेरित होगा, सब प्राणियों के कल्याण में अपने-आप को लगाने में, लोगों को आध्यात्मिक आनन्द की ओर ले जाने में, जगत् को भगवान् की ओर अग्रसर करने के काम में प्रवृत्त होकर जितने दिन उसे इस जगत् में रहना है उतने दिन दिव्य जीवन व्यतीत करेगा। जो भगवत्प्रेमी ऐसा कर सकता है, इस प्रकार सब कुछ को भगवान् के अन्दर आलिंगन कर सकता है, निम्न प्रकृति और त्रिगुणात्मिका माया के सब कर्मों की ओर स्थिर-शांत रूप से देख सकता और बिना क्षुब्ध हुए तथा आध्यात्मिक ऐक्य की ऊँचाई से व्याकुल या च्युत या व्यथित हुए बिना, भगवान् की अपनी दृष्टि की विशालता में स्वतंत्र भाव से रहते हुए, भागवत् प्रकृति की शक्ति से मधुर, महान् और प्रकाशमय होकर उन कर्मों के अन्दर और उन कर्मों पर क्रिया कर सकता है, उसको निःसंकोच परम् योगी कहा जा सकता है। यथार्थ में उसी ने सृष्टि को जीता है, जितः सर्गः।
v.19
योगी के विषय में यह वर्णन व्यक्ति की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें संभव है कि व्यक्ति की बाहरी प्रकृति भी उसके वश में हो परंतु वह एक सीमा तक ही वश में हो सकती है। पुस्तकों में निम्न प्रकृति पर पूर्ण प्रभुत्व के जो वर्णन मिलते हैं, वह स्थिति तो वर्तमान में पार्थिव जगत् में संभव ही नहीं है क्योंकि बिना अतिमानसिक रूपांतर के निम्न प्रकृति को जीता नहीं जा सकता अन्यथा श्रीअरविन्द के अतिमानस की आवश्यकता ही न रह जाती। यह एक मूलभूत बात है। परंतु वर्तमान प्रसंग में हम यह आशा नहीं कर सकते कि भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को योग साधना की बारीकियाँ समझाएँगे जैसा कि श्रीअरविन्द साधकों को लिखे अपने पत्रों में करते हैं। यहाँ योगी की जिस स्थिति का वर्णन किया गया है वह अवश्य ही बहुत हद तक प्राप्त की जा सकती है और यह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस हद तक वह इसे प्राप्त करता है। परन्तु जब तक व्यक्ति निम्न प्रकृति के किसी भी प्रकार के स्पंदनों के प्रति खुला होता है तब तक यह स्थिति पूर्ण रूप से उसमें अक्षुण्ण नहीं बनी रह सकती। अतः संभव है कि आंतरिक प्रकृति में वह शांत बना रहे और यह भी संभव है कि अपनी बाहरी प्रकृति में भी वह बहुत कुछ अविचल बना रहे परंतु मनोवैज्ञानिक रूप से ये आक्रमण न हों, ऐसा हो नहीं सकता हालाँकि उन्हें भी वह अपने तरीके से दूर करने का प्रयास करता है। परंतु ये चीजें किसी को भी नहीं छोड़तीं। श्रीमाताजी ने भी स्वयं अपना अनुभव बताते हुए कहा है कि श्रीअरविन्द के देहत्याग के बाद - जो कि उन्हें मर्म तक स्पर्श करने वाली घटना थी आसुरिक शक्तियों ने उनके ऊपर भयंकर रूप से आक्रमण किया और इस तरीके के सुझाव दिए कि योग-साधना और भगवान् आदि की सब बातें बिल्कुल निरर्थक हैं, और इस पृथ्वी पर कभी भी पूर्णता स्थापित नहीं हो सकती। और इसके साथ ही उन शक्तियों का उन पर इस बात के लिए भयंकर दबाव आया कि वे श्रीअरविन्द आश्रम को ही समाप्त करने की घोषणा कर दें। जब ये शक्तियाँ साक्षात् जगदम्बा तक पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर सकती हैं तब किसी सामान्य व्यक्ति की या फिर किसी योगी की भी क्या सामर्थ्य है कि आसुरी शक्तियों के आक्रमणों से विचलित न हो। हालाँकि श्रीमाताजी से वे ऐसा कुछ भी नहीं करवा सकीं, परन्तु ये शक्तियाँ इस हद तक जा सकती हैं जिससे व्यक्ति अपने मर्म तक विचलित हो सकता है। जब कभी कोई व्यक्ति श्रीमाताजी से निवेदन करता था कि उसके अंदर बहुत से बुरे विचार उठते हैं तब वे कहतीं थीं कि व्यक्ति की अवचेतना में ये सब चीजें होती हैं और वहीं से ये सब विचार उठते रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब श्रीअरविन्द के साथ दुर्घटना घटी तब से कोई भी सप्ताह ऐसा न बीता होगा जब आसुरी शक्तियों ने आकर उन्हें यह सुझाव न दिया हो कि योग आदि को बातें सब निरर्थक हैं। श्रीअरविन्द के शरीर त्यागने के बाद तो इन्होंने यहाँ तक सुझाव दिये कि वे व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रही हैं, इस धरती पर कभी भी भगवान् की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जब ये शक्तियाँ स्वयं श्रीमाताजी को भी आकर विचलित करने का प्रयास कर सकती हैं तो अन्य किसी की तो बात ही क्या है। इसीलिए श्रीअरविन्द ने कहा कि व्यक्ति एक निश्चित सीमा तक संतुलन बनाए रख सकता है परन्तु उस सीमा से परे के संकट या आक्रमण से वह अन्दर तक विचलित हो सकता है। इसीलिए जब श्रीकृष्ण के पैर में तीर लगा वह इस बात का सूचक था कि अधिमानसिक चेतना से भी अवचेतन को जीता नहीं जा सकता। केवल अतिमानस पर पहुँचने पर ही इन चीजों को पराजित किया जा सकता है। उससे नीचे की चेतना में तो अवचेतन का प्रभाव कभी भी व्यक्ति को कम या अधिक विचलित और प्रभावित कर सकता है और मौका मिलते ही चीजों को बिगाड़ सकता है। परंतु गीता का वर्णन प्रस्तुत प्रसंग में बिल्कुल संगत ही है क्योंकि यहाँ हम गीता से योग की व्यावहारिक बारीकियों के वर्णन की आशा नहीं कर सकते।
अर्जुन उवाच
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ।। ३३ ।।
३३. अर्जुन ने कहाः हे मधुसूदन श्रीकृष्ण ! आपके द्वारा जो समत्व-रूप यह योग कहा गया है, मन के चंचल होने के कारण इस योग की मैं (अपने भीतर) दृढ़ स्थिति को नहीं देखता हूँ।
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।। ३४।।
३४. क्योंकि हे कृष्ण ! निश्चय ही मन चंचल स्वभाव का है; यह उग्र, बलवान् और हठीला है; उसके निग्रह करने को मैं वायु को रोकने के समान बहुत अधिक दुष्कर मानता हूँ।
श्रीभगवान् उवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।। ३५।।
३५. श्रीभगवान् ने कहा : हे महाबाहो! निःसंदेह मन चंचल स्वभाव का और बहुत कठिनाई से वशीभूत होनेवाला है; परंतु हे कौन्तेय, वह अभ्यास से और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है।
मनुष्य का मन एक सार्वजनिक स्थान है जो चारों ओर से खुला है, और इस सार्वजनिक स्थान में चीजें आती हैं, जाती हैं, सभी दिशाओं से आर-पार गुजरती हैं; और कुछ वहाँ जम जाती हैं और ये सर्वदा सर्वोत्तम नहीं होतीं। और वहाँ, उस भीड़ के ऊपर नियंत्रण पाना सभी नियंत्रणों में सबसे अधिक कठिन है। अपने मन में आने वाले विचार को संयमित करने का प्रयत्न करो, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम ठीक-ठीक समझ जाओगे कि तुम्हें एक संतरी की तरह, मन की आँखों को पूरा खुला रखकर, किस हद तक चौकसी रखनी पड़ती है, और फिर उन भावों अथवा विचारों के विषय में अत्यंत स्पष्ट दृष्टि रखनी होती है जो तुम्हारी अभीप्साओं के साथ मेल खाती हैं और जो मेल नहीं खातीं। और उस सार्वजनिक स्थान पर जहाँ सभी ओर से सड़कें आकर मिलती हैं, तुम्हें प्रतिक्षण निगरानी रखनी पड़ती है ताकि सभी राह चलते एक साथ भीतर न घुस आयें। यह एक भारी काम है। फिर, यह मत भूलो कि तुम यदि सच्चे प्रयत्न भी करते हो तो भी तुम इन सब कठिनाइयों के अंत तक एक दिन में, एक महीने में, एक वर्ष में नहीं पहुँच जाओगे। जब तुम आरंभ करते हो तब तुम्हें एक अटूट धैर्य के साथ आरंभ करना चाहिये। तुम्हें यह कहना होगा, "भले इसमें पचास वर्ष लगें, भले इसमें सौ वर्ष लगें, यहाँ तक कि चाहे इसमें अनेक जीवन भी क्यों न लगें, तो भी मैं जो कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ उसे मैं अवश्य प्राप्त करूंगा।"
एक बार यदि तुमने ऐसा करने का निश्चय कर लिया, एक बार यदि तुम बिल्कुल सचेतन हो चुके हो कि चीजें ऐसी ही हैं और यह लक्ष्य सतत् और स्थायी रूप से प्रयत्न करने का कष्ट उठाए जाने योग्य है, तो तुम आरंभ कर सकते हो। अन्यथा, कुछ समय बाद तुम क्लांत हो जाओगे; तुम निरुत्साहित हो जाओगे, तुम अपने-आप से कहोगे, "ओह! यह तो बड़ा कठिन है - मैं इसे करता हूँ और यह चौपट हो जाता है, मैं फिर करता हूँ और यह फिर चौपट हो जाता है, और फिर मैं इसे दुबारा करता हूँ और यह हमेशा ही चौपट हो जाता है...। फिर क्या किया जाए? कब मैं वहाँ पहुँचूँगा?" अतएव व्यक्ति में प्रचुर धैर्य होना चाहिये। यह कार्य सौ बार चौपट हो सकता है, और तुम इसे फिर से एक सौ एकवीं बार करोगे, यह हजार बार चौपट हो सकता है और तुम फिर से इसे एक हजार एकवीं बार करोगे जब तक कि अंततः यह चौपट नहीं होगा। और अंत में यह चौपट नहीं होता।
प्राणिक आदान-प्रदान के द्वारा व्यक्ति बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। जैसे कि किसी अवसादग्रस्त व्यक्ति से फोन पर किया शाब्दिक आदान-प्रदान भी हमारे अंदर अवसाद के स्पंदन पैदा कर सकता है, और किसी प्रोत्साहित व्यक्ति से किया आदान-प्रदान प्रोत्साहन के स्पंदन पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि पत्रों के जरिए आदान-प्रदान से भी व्यक्ति बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। शारीरिक रूप से भी ये सत्ताएँ हम पर हमला कर सकती हैं। एक बार श्रीअरविन्द को महसूस हुआ कि कोई उनके ऊपर हमला कर रहा है। पूछताछ करने पर पता लगा कि उनके निवासस्थान से कुछ दूरी पर स्थित कोई व्यक्ति उनके प्रति दुर्भावनाग्रस्त होकर दुश्चिंतन कर रहा था। इसलिए सचेतन व्यक्ति को तो हर कदम पर ही इन विरोधी सत्ताओं और उनके प्रभावों से युद्ध करना होता है। यदि ऐसा न होता तो श्रीअरविन्द को इतनी गंभीर साधना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि उनकी व्यक्तिगत साधना तो उनके जीवन काल में बहुत पहले ही हो चुकी थी। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति को कुछ शांति का अनुभव हो सकता है परन्तु बिना भौतिक रूपांतरण साधित हुए सच्ची पूर्णता संभव नहीं है।
----------------------------------------
* मनुष्य अपने अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी गुप्त तहें, ऐसी छोटी-छोटी चीजें पाता है जो प्रारंभ में उसने नहीं देखी थी; मनुष्य एक प्रकार का आंतरिक पीछा करना शुरू कर देता है, छोटे-छोटे अंधकारपूर्ण कोनों में शिकार खोजने लगता है और अपने-आप से कहता है: "क्या, मैं ऐसा था! यह चीज मेरे अंदर थी, मैंने इस नन्हीं चीज को पोस रखा है!" - कभी-कभी तो वह इतनी गंदी, इतनी नीच, इतनी घिनौनी होती है! और एक बार जब उसका पता लग जाता है, कितना आश्चर्यजनक लगता है! फिर मनुष्य उस पर प्रकाश डालता है और वह विलीन हो जाती है! और फिर उसके बाद तुम में और अधिक वे प्रतिक्रियाएँ नहीं होतीं जो पहले तुम्हें इतना उदास बना दिया करती थीं, जब तुम कहा करते थे, "ओह! मैं कभी वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा।" उदाहरणार्थ, तुम एक बहुत साधारण-सा (ऊपर से देखने में बहुत साधारण) संकल्प करते होः "मैं अब कभी कोई झूठी बात नहीं कहूँगा।" और अकस्मात्, तुम्हारे बिना जाने कि क्यों और कैसे, झूठो बात बिल्कुल अपने-आप निकल पड़ती है और तुम उसे तब देखते-जानते हो जब वह मुँह से निकल चुकी होती है। तुम कहते हो: "यह तो सही बात नहीं है जो मैंने अभी कहा है: मेरा मतलब तो कोई और ही बात कहने का था।" अतः तुम खोजते हो, खोजते हो यह कैसे घटित हुआ? मैंने कैसे उस ढंग से सोचा और वैसा कह दिया? कौन-सी चीज मेरे अंदर से बोली, किसने मुझे धक्का दे दिया?" तुम स्वयं को बिल्कुल संतोषजनक व्याख्या दे सकते और कह सकते हो, "यह चीज बाहर से आयी थी" अथवा "यह अचेतनता का एक क्षण था", और इस विषय में और कोई बात न सोचो। और दूसरी बार फिर वही शुरू हो जाता है। इसकी बजाय, तुम इस प्रकार खोजते हो, "उस व्यक्ति का क्या उद्देश्य हो सकता है जो झूठ बोलता है?..." और तुम आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ते हो और एकाएक तुम एक छोटे-से कोने में एक ऐसी चीज को खोज निकालते हो जो अपने-आपको सही सिद्ध करना चाहती है, स्वयं को आगे रखना चाहती है अथवा देखने के अपने निजी तरीके को स्थापित करना चाहती है (चाहे जो भी हो उससे कुछ आता-जाता नहीं, उसके कई कारण हो सकते हैं), अपने-आपको उससे थोड़ा भिन्त्र रूप में दिखाना चाहती है जो वह है, ताकि लोग तुम्हारे विषय में थोड़ी अच्छी राय बनायें और यह समझें कि तुम कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति हो...। बस, यही चीज थी जो तुम्हारे अंदर बोल पड़ी थी - तुम्हारी सक्रिय चेतना नहीं, अपितु वही चीज जो वहाँ थी और जिसने तुम्हारी चेतना को पीछे से धक्का दिया था। जब तुम एकदम सावधान नहीं थे, इसने तुम्हारे मुँह का, तुम्हारी जीभ का उपयोग कर लिया, और तब तुम सचेत हुए! झूठ निकल पड़ा। मैं तुम्हें यह उदाहरण दे रही हूँ - लाखों-लाखों दूसरे उदाहरण हैं। और यह सब अत्यंत मजेदार है। और जिस हद तक मनुष्य अपने अंदर इस चीज को खोज निकालता है और सच्चाई के साथ कहता है, "इसे अवश्य बदलना चाहिये", वह पाता है कि वह एक प्रकार की आंतरिक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर रहा है, वह क्रमशः इस विषय में सचेतन होता जाता है कि दूसरों में क्या घटित हो रहा है, और जब वे बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसा कि वह उन्हें देखना चाहता है तो वह क्रोध से आग-बबूला होने के बदले यह समझना आरंभ कर देता है कि चीजें कैसे घटित होती हैं, क्या कारण है कि मनुष्य "इस प्रकार का" है, प्रतिक्रियाएँ कैसे उत्पन्न होती हैं!.....तब, ज्ञान से संतुष्ट होकर वह मुस्कुराता है। वह अब कठोरतापूर्वक आँकलन अथवा निर्णय नहीं करता, वह अपने अंदर की या दूसरों के अंदर की कठिनाइयों को, चाहे उनकी अभिव्यक्ति का केंद्र कुछ भी क्यों न हो, दिव्य 'चेतना' को समर्पित कर देता है, और उसके रूपांतर के लिए प्रार्थना करता है।
अधिकतर सिद्धियों और समता आदि की जो चर्चाएँ हमारे पढ़ने-सुनने में आती हैं वे केवल एक निश्चित दायरे में ही होती हैं और निश्चित तरीके के नियमों का पालन कर के ही बनाए रखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि अवतारों आदि की, जिनकी आंतरिक सत्ता बहुत प्रबल होती है, उन्हें भी बाहरी रूप से तो उनके जीवन में हम समय-समय पर विचलित होते हुए देख सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर ही हमें समझ में आता है कि श्रीअरविन्द और श्रीमाताजी जिस चीज की ओर संकेत कर रहे हैं वह कोई आंशिक चीज नहीं अपितु मूलभूत और पूर्ण चीज है। गीता यहाँ जिन स्थितियों का वर्णन कर रही है उनका सही परिप्रेक्ष्य हमें केवल श्रीअरविन्द की व्याख्या से ही मिलता है अन्यथा तो हम उसे ही एक पूर्ण चीज मान बैठने की भूल कर सकते हैं जैसा कि अधिकांशतः होता ही है।
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवासुमुपायतः ।। ३६।।
३६. जो मनुष्य आत्म-संयमित नहीं है, उसके लिये इस योग को प्राप्त करना कठिन है; किंतु आत्म-संयमित व्यक्ति द्वारा, उचित उपाय से प्रयत्न करते रहने पर, इसे प्राप्त करना संभव है, ऐसा मेरा मत है।
क्योंकि, हमारी सारी प्रकृति तथा इसकी परिस्थिति, हमारी समस्त व्यक्तिगत एवं समस्त विश्वगत सत्ता कुछ ऐसे अभ्यासों और प्रभावों से परिपूर्ण है जो हमारे आध्यात्मिक नवजन्म के प्रतिकूल हैं और हमारे पुरुषार्थ की एकनिष्ठता का भी विरोध करते हैं। किसी अर्थ में हम उन मानसिक, स्नायविक और शारीरिक अभ्यासों के एक जटिल पुंज के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं जिसे हमारे कुछ प्रधान विचारों, कामनाओं और संसगों ने एक-दूसरे के साथ जोड़े रखा है, - एक ऐसा अनेकानेक छोटी-छोटी पुनरावर्ती शक्तियों का मिश्रण जिसमें कुछ एक प्रधान स्पंदन रहते हैं।
व्यक्ति के अंदर अनेकानेक छोटी-छोटी विरोधी चीजें होती हैं जो उसकी अवचेतना की गहराई में छिपी होती हैं। जब व्यक्ति साधना में प्रकाशपूर्ण क्षणों में होता है, उसकी आत्मा बहुत प्रबल होती है और जब तक उसके अन्दर श्रीमाताजी के प्रति बहुत भक्ति होती है तब तक वे छोटी-छोटी चीजें चुपचाप कोनों में छिपी रहती हैं और अपना सिर नहीं उठातीं क्योंकि वे जानती हैं कि व्यक्ति के अन्दर भगवान् की भक्ति का प्रकाश फैला हुआ है। परन्तु उन छोटी-छोटी चीजों का समाधान किये बिना यदि यही प्रकाशपूर्ण अवस्था बनी रहती तो यह तो बड़ी संकटपूर्ण बात होती क्योंकि ये हिस्से तो आत्मा के प्रकाश में कभी सामने आ ही नहीं पाते। इसलिए भगवान् ने उन्हें उद्घाटित कर के प्रकाश में लाने की बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा संकट आता है जिससे वह मर्म तक विचलित हो जाता है, उसका सहज संतुलन भंग हो जाता है और उसका विश्वास डगमगा जाता है, वैसे ही ये चीजें अपना सिर उठा लेती हैं और अपना प्रभाव डालती हैं। ऐसे में जो सच्चा साधक है वह इसे भागवत् कृपा के रूप में लेता है जो कि उसे इन छिपी हुई चीजों के विषय में अवगत कराती है और वह उस कृपा के सहारे अपने इन हिस्सों को साफ करने का प्रयास करता है। हालाँकि इसका यह अर्थ नहीं है कि जब व्यक्ति सचेतन हो जाता है तब प्रकृति की समस्याएँ हल हो जाती हैं। केवल श्रीअरविन्द और श्रीमाँ ही इन चीजों की बारीकियों के बारे में चर्चा करते हैं। उनके कथन के अनुसार जब तक अवचेतन और निश्चेतन है तब तक इन समस्याओं का सच्चा निराकरण नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति जितना ही अधिक ऊँचाई पर आरोहण करता जाता है उतनी ही अधिक गहरी सफाई वह अपने निम्नतर भागों की कर सकता है। और जड़-भौतिक तत्त्व में अतिमानसिक रूपांतर के बिना पूर्ण रूप से इन हिस्सों की सफाई हो भी नहीं सकती। उससे पहले तो ये सभी छोटी-छोटी विरोधी चीजें अन्दर घात लगाकर बैठी रहती हैं और मौका मिलते ही हमला कर देती हैं। यह कोई हतोत्साहित होने की बात नहीं है। इसमें सही दृष्टिकोण यह है कि पहले हमारी वर्तमान स्थिति का हम सही जायजा लें और बिना धीरज खोए अपनी सफाई का काम आरंभ करें और सदा ही यह ध्यान में रखें कि यह कार्य बहुत ही कठिन है। हमारी आंतरिक चेतना इसमें सहायक होती है। वह किन्हीं भी बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होती और अवचेतना भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए जब व्यक्ति उसमें निवास करता है तब वह इन चीजों के साथ विजयी रूप से व्यवहार कर सकता है अन्यथा तो उसके पास पाँव जमाने के लिए भी कोई जगह नहीं होती।
इसके लिए पहली आवश्यकता है कि मन की उस केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि को विलीन कर दिया जाए जो उसे अपने विकास एवं तुष्टि तथा पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस-लाभ करने में तल्लीन रखती है। यह अत्यावश्यक है कि इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर उस गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए जो एकमात्र भगवान् को ही देखती है और केवल भगवान् की ही खोज करती है। दूसरी आवश्यकता है कि हमारी समस्त निम्नतर सत्ता को इस नवीन श्रद्धा तथा महत्तर दृष्टि के प्रति नतमस्तक होने को बाध्य किया जाए। हमारी संपूर्ण प्रकृति को पूर्ण समर्पण करना होगा; इसे स्वयं को अपने प्रत्येक भाग तथा अपनी प्रत्येक गति में उस वस्तु के प्रति सौंप देना होगा जो असंस्कृत इंद्रियबद्ध-मन को स्थूल संसार और इसके पदार्थों की अपेक्षा बहुत ही कम यथार्थ प्रतीत होती है। हमारी संपूर्ण सत्ता को - अंतरात्मा, मन, इंद्रिय, हृदय, इच्छाशक्ति, प्राण और शरीर को - अपनी सभी शक्तियों का अर्पण इतनी पूर्णता के साथ तथा ऐसे तरीके से करना होगा कि वह भगवान् का उपयुक्त वाहन बन जाए। यह कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु अपनी नियत प्रवृत्ति का, जो उसके लिए एक नियम स्वरूप होती है, अनुसरण करती है और किसी मौलिक परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। और, अन्य कोई भी परिवर्तन उतना मौलिक नहीं होगा जितना कि वह क्रांतिस्वरूप परिवर्तन जिसका पूर्ण योग में प्रयास किया जाता है। हमारे अंदर की सभी चीजों को सतत् केंद्रीय श्रद्धा, संकल्प तथा दृष्टि को ओर मोड़ना पड़ता है। प्रत्येक विचार और आवेग को उपनिषद् की भाषा में यह स्मरण कराना होता है कि "दिव्य ब्रह्म वह है, न कि यह जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं।"
इसमें समर्पण के विषय में बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है जो कि साधना का सार है और इस समर्पण के लिये क्या किया जाये यह समझना बहुत आवश्यक है।
प्रश्न : श्रद्धा, आन्तरिक श्रद्धा और केन्द्रीय श्रद्धा में क्या अन्तर है?
उत्तर : श्रद्धा तो मूलतः एक ही होती है, बस इसकी ये तीन अभिव्यक्तियाँ हैं। जब आत्मा द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है तब वह केन्द्रीय श्रद्धा होती है, जब आन्तरिक सत्ता द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है तब आन्तरिक और बाहरी सत्ता में जब वह प्रकट होती है तब उसे केवल श्रद्धा का नाम दे देते हैं। वास्तव में तो श्रद्धा एक ही है।
आखिर हम संसार में क्यों फँसे हैं? क्योंकि हमारी श्रद्धा सांसारिक क्रियाकलापों - खाने-पीने, सोने-जागने, हँसने - रोने आदि पर ही केन्द्रित है क्योंकि बिना श्रद्धा के तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अतः वर्तमान में हमारी श्रद्धा हमें बाहरी चीजों में लगाए रखती है या यों कहें कि हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति वर्तमान में इसी प्रकार से हो रही है। संसार हमें जिस प्रकार का प्रतीत होता है वह हमें हमारी श्रद्धा के प्रभाव से ही वैसा दिखाई देता है। हमें बाहरी चीजों में प्रवृत्त इस श्रद्धा को मिटाना होगा और इसे आन्तरिक श्रद्धा से प्रतिस्थापित करना होगा, क्योंकि जब तक हमारी श्रद्धा किसी गहरी चीज में नहीं होगी तब तक हम इस संसार से ऊपर नहीं उठ सकते। संसार में श्रद्धा के अतिरिक्त अन्य कोई नियम या विधान नहीं है। सभी कुछ तो श्रद्धा की ही अभिव्यक्ति है। श्रद्धा सर्वशक्तिमान् है। इसीलिए हमें अपनी बाहरी श्रद्धा को तोड़ना होगा और वह तभी संभव है जब हमारी श्रद्धा किसी गहरी वस्तु पर होगी। जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसा ही संसार हमें नजर आयेगा। श्रद्धा ही सब कुछ का निर्माण करती है।
अतः श्रीअरविन्द कहते हैं कि यह अत्यावश्यक है कि इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर उस गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए जो एकमात्र भगवान् को ही देखती है और केवल भगवान् की हो खोज करती है। जब तक हम आन्तरिक श्रद्धा के प्रति नहीं खुल जाते और अपने अहं की तुष्टि में ही लगे रहते हैं तथा हमारा मन हमारे इन नाना प्रकार के अहं-केन्द्रित तर्कों का ही समर्थन करता रहता है तब तक हमारा जीवन उन्हीं चक्करों में लगा रहेगा। इसलिये यदि हमें इससे निकलना है तो हमें इस बाहरी श्रद्धा को उस पवित्रतर श्रद्धा से प्रतिस्थापित करना होगा जिसकी आत्म-अभिव्यक्ति हमारे अंदर है। हम श्रद्धा की ऐसी गहराइयों में जा सकते हैं जो केवल परमात्मा को ही देखती है और उन्हें ही चाहती है और तभी हम इस सतही श्रद्धा को मिटा सकते हैं। बिना गहरी श्रद्धा के आए हम वस्तुओं में लिप्त इस सतही श्रद्धा को मिटा नहीं सकते। यदि व्यक्ति भगवान् की ओर गति करने का दबाव या प्रेरणा महसूस करता है तो ऐसा वह उस आन्तरिक श्रद्धा के प्रभाव के कारण ही करता है। यह इस चीज का सूचक है कि वह आन्तरिक सत्ता हमें संदेश भेज रही है और अपनी उपस्थिति महसूस करा रही है। वर्तमान में हमारी सारी सत्ता काम-पुरुष के इर्द-गिर्द ही केंद्रित है, हालाँकि काम-पुरुष भी हमारी केंद्रीय सत्ता का ही भ्रष्ट रूप है, इसलिए हम बाहरी चीजों से ही संतुष्टियाँ बटोरने में लगे रहते हैं। परन्तु आंतरिक श्रद्धा के प्रभाव से आते संदेश तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि हम सतही चीजों में अपनी श्रद्धा को खत्म न कर दें। और यह तभी संभव है जब हमें अपने सभी क्रिया-कलापों के पीछे श्रीमाताजी की क्रिया नजर आने लगे और हम केवल उन्हीं के लिये कार्य करने लगें। अन्यथा यह सम्भव नहीं है। हमारे ऊँचे से ऊँचे आदर्श भी केवल हमारे अहं के ही रूप हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल भगवान् को प्राप्त करना होना चाहिये और उनकी सेवा करना होना चाहिये।
इसके लिये हमें अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना होगा। भगवान् हमसे हमारी क्षमता से अधिक की माँग नहीं करते। किसी भीषण संकट से उबरने के लिए या फिर अपनी किसी रुचिकर वस्तु को प्राप्त करने के लिये हम जितनी ऊर्जा लगाते हैं उतनी ही ऊर्जा हमें भगवान् को प्राप्त करने के लिये लगानी होगी और उस चेतना में जाना होगा जिसमें हम केवल भगवान् को ही देखें और केवल उन्हें ही चाहें। यह पहली शर्त है। यह उनके लिए लागू होती है जिनके मन में यह पहले ही आ चुका है कि उन्हें भगवान् को प्राप्त करना है।
इसके बाद जिस दूसरी चीज की आवश्यकता है वह है इच्छा-शक्ति, संकल्प-शक्ति, क्योंकि हमारी सतही प्रकृति सहज ही इस निर्णय को स्वीकार नहीं करने वाली है। उसकी लिप्तता तो संसार की अनेकों प्रकार की कामनाओं में रहती है। इसलिये हमें पूरी संकल्प-शक्ति के साथ अपनी सतही प्रकृति को बाध्य करना होगा कि वह इस केन्द्रीय श्रद्धा के प्रति नतमस्तक हो, उसकी अधीनता स्वीकार करे।
अतः पहली चीज है वह केन्द्रीय श्रद्धा जो हमेशा श्रीमाँ को ही देखती है और केवल उन्हें ही चाहती है। और दूसरी है, हमारी बाहरी प्रकृति को हमारी इस केन्द्रीय श्रद्धा के प्रति नतमस्तक होने के लिए बाध्य करना। जब हम केवल श्रीमाँ को ही चाहेंगे तो हमें मार्ग पर दृढ़ बने रहने के लिये अधिकाधिक शक्ति प्राप्त होती जाएगी और हम संघर्षों को पार कर के अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसमें कितना समय लगेगा वह अलग-अलग होता है और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। परन्तु सच्ची बात तो यह है कि हमारे भीतर श्रीमाँ के प्रति भाव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भाव ही ना रहे जो कि हम पर अपना अधिकार जमा ले, भले ही वह भाव समाज के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो या अपने ऊपर किये गये किसी उपकार की कृतज्ञता का हो। श्रीमाताजी को छोड़कर अन्य कोई कर्तव्य का भाव ही न रहे। क्योंकि सामान्यतया जिसे हम कर्तव्य कहते हैं वह तो विवेकानंदजी के अनुसार एक ऐसा रोग है जो हमारी आत्मा को झुलसा देता है। कर्त्तव्य, कृतज्ञता आदि तब तक बहुत सहायक होते हैं जब तक कि व्यक्ति अपनी निम्न प्रकृति के ही वश में होता है और उसकी आत्मा इतनी प्रबल नहीं होती कि सचेतन रूप से उसके बाहरी हिस्सों पर अपना अधिकार कर सके। अवश्य ही कृतज्ञता एक आंतरिक गुण है। परन्तु जब हम साधना के मार्ग पर चलते हैं तब हम यह जान जाते हैं कि सभी शरीरों में स्वयं श्रीमाँ ही विद्यमान हैं और वे ही किसी एक के या दूसरे के माध्यम से हमारी सहायता करती हैं। इसलिये यह अनुभव होने के बाद हम उस माध्यम विशेष से नहीं अपितु स्वयं श्रीमाँ के प्रति ही गहरी कृतज्ञता का भाव अनुभव करने लगते हैं जहाँ से कि हमें सभी अनुग्रह वास्तव में प्राप्त होते हैं।
परंतु सतही श्रद्धा को मिटाकर इस गहरी श्रद्धा को स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि ऐसा करने में प्रकृति तरह-तरह के सुझाव देती है, भाँति-भाँति के छलावे करती है और हमें मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करती है। वह हमारे समक्ष कर्तव्य-अकर्त्तव्य के बोध रखती है, धर्म-अधर्म के विचार रखती है और उनका निष्ठापूर्वक पालन करने को बाध्य करती है। इसलिये जब तक हम अपने इन सामान्य धर्मों को तोड़ नहीं देते तब तक वास्तव में भगवान् की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। हमारी पूर्व में बनी हुई धारणाओं को टूटने में भी बहुत समय लग जाता है और यह समय की अवधि व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर करती है। किसी-किसी को तो अपेक्षाकृत कम समय लगता है, वहीं किसी-किसी की पचासों वर्ष लगाने पर भी आवश्यक नहीं कि पूर्व में बनी धारणाएँ टूट जाएँ। इसलिये आत्मा के दृष्टिकोण से कर्तव्य-अकर्तव्य, धर्म-अधर्म आदि के सभी बोध अंधकारस्वरूप ही हैं जिसकी सहमति न तो गीता देती है और न ही श्रीअरविन्द । क्योंकि यदि बारीकी से देखा जाए तो हमारे सारे कर्त्तव्यबोध और हमारे कृतज्ञता के बोध अंततोगत्वा हमारे शरीर के संबंध से या अधिक-से-अधिक हमारे बाहरी व्यक्तित्व के संबंध से ही तो होते हैं। जबकि सच्चे दृष्टिकोण से सभी चीजें तो श्रीमाँ के संबंध से होनी चाहिये। कृतज्ञता तो हमें उन्हीं के प्रति रखनी चाहिये और कर्तव्य भी हमारा उनके अतिरिक्त अन्य किसी के लिए नहीं होना चाहिये। इसीलिये योगी श्रीकृष्णप्रेम कहते थे कि भगवान् के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखना तो भ्रमपूर्ण रूप से देखने के ही भिन्न-भिन्न तरीके हैं। कृतज्ञता का बोध तो तब सहायक है जब कोई निम्न वृत्ति सिर उठाये या किसी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भाव उठे तब कृतज्ञता का बोध हमें यह याद दिलाता है कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ अमुक समय कोई हितैषिता का व्यवहार किया था। इसीलिये समाज में इन गुणों का इतना महत्त्व है ताकि ये मनुष्य की निम्न प्रकृति को हावी होने से रोक सकें। इसी के लिए भारतीय संस्कृति ने सापेक्ष धर्मों का निर्माण किया था। परंतु ये सभी बाहरी धर्म उस पर और अधिक प्रभावी नहीं होते जिसने अपनी आत्मा के विधान को स्वीकार कर लिया होता है।
कर्तव्य बोध तथा कृतज्ञता के भाव की जितनी भी बातें होती हैं वे सभी प्रायः हमारी निम्न प्रकृति पर कुछ अंकुश लगाने के लिये होती हैं ताकि हम अतिशय रूप से स्व-केंद्रित न हो जायें। ये चीजें हमारी आत्मा की निम्न प्रकृति से रक्षा करती हैं। जो व्यक्ति स्व-केंद्रित होता है उसके लिये अपने माता-पिता की सेवा करने का कर्त्तव्य बहुत आवश्यक है। परंतु ये ही सुझाव उस व्यक्ति के लिये बंधनस्वरूप और बाधक हो जाते हैं जिसने परमात्मा के प्रति समर्पण करने का दृढ़-संकल्प कर लिया है। सामान्य दृष्टिकोण से तो यह एक बहुत ही उच्च भाव है कि जब कोई हमारा थोड़ा भी भला करे तो उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता रखना और उसी के अनुरूप व्यवहार करना। परन्तु जब हमने श्रीमाँ के प्रति सच्चा समर्पण कर दिया होता है तब फिर हमारा सारा जीवन, हमारे सारे साधन, सारे प्रयास, सारे कर्तव्य, सारी कृतज्ञता अनन्य रूप से केवल उन्हीं के प्रति निवेदित हो जाते हैं। क्योंकि वे ही हैं जो सभी में तथा सर्वत्र विराजमान हैं और जो कुछ भी होता है और जिसके द्वारा भी होता है उस सब के पीछे एकमात्र उन्हीं का हाथ होता है। इसलिये जब हम श्रीमाँ के प्रति समर्पित होते हैं तब फिर अन्य कोई अहंपरक कर्तव्यबोध अथवा किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता के लिये तो कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसीलिए बाहरी चीजों में लिप्त श्रद्धा को बाध्य करना होगा कि वह आंतरिक श्रद्धा की अधीनता स्वीकार करे। सभी कर्मों के लिये एक ही मापदंड है कि हमें सभी मिथ्यात्व, मोह, भ्रांति आदि के सुझावों को एक ओर रख कर पूर्ण सच्चाई के साथ और हमारी चेतना के उच्चतम संभव शिखर पर स्थित होकर केवल यह देखना होगा कि हमारे अमुक कार्य से श्रीमाँ प्रसन्न होंगी या नहीं। वही चीज जो पहले हमें हमारी निम्न प्रकृति से ऊपर उठने में मदद करती थी, उसका उपयोग समाप्त हो जाने पर समर्पण के मार्ग में बाधा बन जाती है चाहे वह अहं हो, चाहे तर्क-शक्ति हो, चाहे ज्ञान हो अथवा चाहे अन्य कुछ भी क्यों न हो। क्रमविकास में ये ही सभी पाशविकता से उठकर हमारे मानव व्यक्तित्व के निर्माण में तो एक सीमा तक सहायक होते हैं परंतु जब इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तब ये ही बाधा बन जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए इन सब को तोड़ना होता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में यह सर्वमान्य रहा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति संन्यास धर्म अपनाता है वैसे ही उसके सभी धर्म, कर्त्तव्य, बंधन आदि नष्ट हो जाते हैं और वह उन सबसे मुक्त होकर आत्मोत्सर्ग के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। उसके बाद उस पर अपने संन्यास धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई कर्तव्य बाध्यकारी नहीं रहता। परंतु श्रीअरविन्द के योग में चूँकि बाहरी संन्यास का कोई विधान नहीं है इसलिये व्यक्ति कहता तो है कि वह भगवान् की ओर जाना चाहता है, साधना करना चाहता है, श्रीअरविन्द व श्रीमाँ का योग करना चाहता है, परंतु फिर भी लंबे समय तक या फिर जीवनपर्यंत भी वह अपने बाहरी कर्तव्यों के निर्वाह में ही लिप्त रहता है और उस चक्कर से नहीं निकल पाता। हालाँकि इसका यह अर्थ नहीं है कि संन्यास ही एकमात्र उपाय है और व्यक्ति को अपने परिवार आदि को त्याग देना आवश्यक है। परंतु इसमें सच्चा मनोभाव यह है कि अपने परिवार आदि को भी श्रीमाँ को सौंप दिया जाए। तभी परिवार का भी सच्चा कल्याण हो सकता है। यदि व्यक्ति अपने अहं के कारण परिवार का पोषण करने की बजाय श्रीमाँ की इच्छानुसार उनका निर्वाह करता तब तो उसमें अहं की नहीं बल्कि दिव्य क्रिया प्रभावी हो जाती है। हालाँकि व्यक्ति योजना बना कर यह काम नहीं करता कि ऐसा करने से उसके परिवार का भला हो जाएगा। परंतु श्रीमाँ के प्रति उत्सर्ग होने पर यह तो उसका एक सहज परिणाम है। इसके कुछ उदाहरण हमें स्वयं श्रीअरविन्द आश्रम में ही मिलते हैं और बाहर तो इसके अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं कि किस प्रकार जिसने अपने-आप को पूर्ण रूप से भगवान् को अर्पित कर दिया उसके परिवार तक का योगक्षेम भगवान् स्वयं ही वहन करते हैं। कर्त्तव्य आदि की बातों पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए श्री दिलीप कुमार रॉय द्वारा लिखे एक पत्र के प्रत्युत्तरस्वरूप श्रीअरविन्द ने जो उत्तर दिया वह बड़ा ही प्रेरक है। श्री दिलीप ने लिखा : पूर्वी बंगाल में १९४६ में हजारों हिन्दुओं का कत्ल व उनकी स्त्रियों से बलात्कार किया गया, उनके घरों को जलाया गया और उनकी लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था। मैंने बहुत दुखित अनुभव किया, इसलिए अधिक क्योंकि मेरे अनेक मित्र मुझे शोक-संतप्त हिन्दुओं के लिए राहत कार्यों की भीषण तात्कालिक आवश्यकता के विषय में लिखते रहते थे। "गुरु, क्यों नहीं आप मुझे राहत कर्मियों का साथ देने के लिए जाने देते?" ..."मेरे पास खोने को कुछ नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ समय से मैं आपके योग में भी अधिक कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए प्रायः इन दिनों मुझे १९३८ का टैगोर का कथन याद आता है: 'दिलीप, तुम और मैं स्वभाव से कलाकार हैं, योगी नहीं।' इसलिए क्या आप मुझे जाने की इज़ाज़त देंगे?" इसके उत्तर में श्रीअरविन्द ने लिखा : "तुम्हारी वर्तमान स्थिति, जिसे मैं पूरी तरह से समझता हूँ, का तुम्हारा ब्यौरा पाकर मेरी सलाह तुम्हें वही हैः ऊषा के आने तक दृढ़ता से लगे रहो - वह अवश्य ही आएगी यदि तुम किसी बाहरी अंधकार में भाग छूटने के प्रलोभन को रोके रखो जहाँ पहुँचने में उसे बहुत अधिक कठिनाई होगी। ....ये ऐसी चीजें हैं जो लगभग अवश्यंभावी रूप से किसी-न-किसी मात्रा में किसी विशिष्ट निर्णायक अवस्था में आती ही हैं जिससे होकर लगभग सभी को गुजरना होता है और जो कष्टदायक रूप से एक लंबे समय तक चलती है परंतु यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि वह निर्णायक या अंतिम हो। सामान्यतया, यदि कोई दृढ़ता से लगा रहता है, तो गहनतम अंधकार की रात्रि की अवधि लगभग प्रत्येक आध्यात्मिक अभीप्सु को ऊषा से पहले आती ही है। यह इस कारण आती है क्योंकि व्यक्ति को बिना किसी सच्चे मानसिक प्रकाश या जीवन में किसी प्रकार के हर्ष के सहारे के ही घोर भौतिक चेतना में निमग्न होना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें सामान्यतया आवरण के पीछे चली जाती हैं, हालाँकि, जैसा कि प्रतीत होता है वैसे, वे स्थायी रूप से खो या छूट ही नहीं जातीं। यह एक ऐसी अवधि है जब संदेह, इन्कार, शुष्कता, म्लानता और इसी के जैसी चीजें बड़े भारी वेग के साथ उभर आती हैं और कुछ समय के लिए प्रायः पूरी तरह से आधिपत्य रखती हैं। इस अवस्था को सफलतापूर्वक पार कर लिये जाने के बाद ही सच्चा प्रकाश आने लगता है, वह प्रकाश जो मन का नहीं अपितु आत्मा का होता है। निःसंदेह प्रारंभिक अवस्थाओं में कुछ हद तक आध्यात्मिक प्रकाश आता है और कुछ को तो काफी हद तक आ जाता है, हालाँकि ऐसा सभी के साथ नहीं होता - क्योंकि कुछ को तो तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक कि वे अपनी मानसिक, प्राणिक और शारीरिक चेतना में से अवरोधनकारी पदार्थ को हटा न दें, और तब तक उन्हें उसका केवल यदा-कदा ही एक संस्पर्श प्राप्त होता है। परंतु अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी, यह आरंभिक आध्यात्मिक प्रकाश कभी भी पूर्ण नहीं होता, जब तक कि भौतिक चेतना के अंधकार का सामना कर उसे विजित न कर लिया गया हो। ऐसा नहीं कि कोई अपनी गलती के कारण इस अवस्था में गिर जाता है; यह तब भी आ सकती है जब साधक आगे बढ़ने के लिए अपना अधिकतम प्रयास कर रहा होता है। यह वास्तव में प्रकृति में कोई मूलभूत अयोग्यता को नहीं दर्शाता परंतु अवश्य ही यह एक कठिन परीक्षा है और साधक को इससे गुजरने के लिए बड़ी सुदृढ़ता से लगे रहना होता है। इन चीजों को समझाना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को समझना या उसे स्वीकार करना सामान्य मानव तर्क-बुद्धि के लिए कठिन है। मैं ऐसा करने का प्रयास करूँगा परंतु इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। तब तक, जैसा कि तुमने मेरी सलाह चाही है, मैं तुम्हें यह संक्षिप्त उत्तर भेजता हूँ।"
इसी पत्र की प्रतिक्रिया में श्रीकृष्णप्रेम ने लिखा: "अपने मन को श्रीकृष्ण के चरणों में लगाए रखो, सदा यह याद रखो कि तुम 'उनके' हो न कि अपने-आप के और चाहे प्रकाश में हो या अंधकार में, हर्ष में हो या शोक में, जैसा 'वे' चाहें उसी तरह बस चलते रहो....तुम्हारे पुराने जीवन में लौट जाने के विचार को क्षण भर के लिए भी तूल न दो : वह अब सदा के लिए जा चुका है और उसके संबंध में विचार परेशानी के अलावा और कुछ नहीं ला सकते। ये चीजें कभी न कभी तो आती ही हैं - और अधिकांश के लिए तो - और मुझे लगता है वास्तव में तो सभी साधकों के लिये - कभी - कभी बार-बार आती रहती हैं। रूप भिन्न हो सकता है परंतु कारण समान ही रहता है : आत्मा की ऊर्ध्व-गति में हमारी 'निम्न प्रकृतियों' पर राज करने वाली शक्तियों का विरोध। स्वाभाविक रूप सं, जब वह ऊर्ध्व-गति सच्ची होती है या जिसके सच होने का पूरा विश्वास होता है केवल तभी उन शक्तियों को अपना राज्य खतरे में लगता है या फिर वे किसी न किसी प्रकार के तूफानों और अंधकार के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया देती हैं। यही नहीं, वे ऐसा केवल हमारे अंदर की किसी कमजोरी, या कुंठित कामनाओं से जन्मे आंतरिक रोष या विषाद को काम में लेकर ही कर सकती हैं। जैसे जादूगर को अपने जादू कर सकने के लिये अपने होने वाले मोहरे की किसी चीज की जरूरत होती है - कोई बालों का गुच्छा या कपड़े का टुकड़ा - उसी प्रकार इन शक्तियों को अपनी माया कर सकने के लिये हमारे अंदर आधारस्वरूप किसी कमजोरी की आवश्यकता होती है। जब भी इस प्रकार के विचार उभर कर आएँ तभी श्रीकृष्ण के चरणों का ध्यान-चिंतन करते हुए इन्हें अपने से दूर रखो। और उन्हें तुम्हारे अपने विचार मानने से मना करो और यह अनुभव करो कि वे बाहर से आते हैं और फिर 'उनके' चरणों से जगमगाने वाली ज्योति को उन्हें छितराकर दूर भगाने दो। तब फिर यह खोजो कि तुम्हारे अंदर वह कौन-सी चीज है जिसे आधारबिंदु बनाकर उन्होंने तुम्हारे अंदर क्रिया की - यह लगभग सदा ही अहं की कोई कुंठित कामना ही होती है जो प्रायः सतही मन द्वारा सर्वथा उपेक्षित होती है।
"बहरहाल, जिस भी तरह हो, बस इससे लगे रहो, चिपके रहो, पीछे मुड़ने की तो सोचो भी मत। जिस क्षण तुमने ऐसा किया (अर्थात् पीछे मुड़े) उसी क्षण अपने प्रयोजन में पुष्ट होकर ये शक्तियाँ अपना माया-जाल छोड़ देंगी और तुम बड़े भारी रूप से अफ़सोस करोगे।
"हमारे लिए कोई प्रत्यावर्तन या पीछे मुड़ना हो ही नहीं सकता, दिलीप : हमने जो पीछे छोड़ दिया है वह नष्ट हो चुका है और यह सोचना निरा भ्रम है कि हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वह जा चुका है और भले हमें अच्छा लगे या न लगे, शोक में हो या हर्ष में, हमें चलते ही रहना होगा। यहाँ तक कि पीछे मुड़ने की कोशिश भी मत करो ऐसा करना केवल हमारे मस्तिष्क को चकरा सकता है और हमें जो नजर आती हैं वे केवल छलपूर्ण मृगमरीचिकाएँ हैं।
"इसकी बजाय हमें उस भविष्य की ओर निहारना चाहिये जिसमें वर्तमान में जो है उससे सर्वथा भिन्न चीज का आश्वासन निहित है। अब इसी क्षण हमें कृष्ण के शाश्वत चरणों को थाम लेना चाहिये और भविष्य में किसी दिन उन्हें थामने की आशा न करें - 'यदि हम अच्छे रहे तो जैसा कि वे हमें तब बताते थे जब हम बच्चे थे। अभी, अभी, अभी! अतीत को जाने दो और भावी को अपनी चिंता खुद करने दो।
"यह स्वाभाविक ही है कि तुम बंगाल की भयावह स्थितियों से बड़े कष्टमय रूप से प्रभावित होवोगे परंतु वह भी तो कृष्ण के ही हाथों में है। जिसने-अपने आप को कृष्ण के हाथों में सौंप दिया है उसे तो अटल रूप से उन्हीं के चरणों में अपनी नजरें रखनी चाहिये चाहे तीनों लोक विध्वंस में ही क्यों न जा गिरें।"
इस पत्र की प्रतिक्रियास्वरूप श्रीअरविन्द ने लिखा : "कृष्णप्रेम का पत्र शुरू से अंत तक सराहनीय है और हर वाक्य महत् अर्थसंगतता और बल के साथ सत्य से जा टकराता है। प्रत्यक्ष रूप से उन्हें योग में कार्य करने वाली मनोवैज्ञानिक और गुह्य ताकतों का एक सटीक ज्ञान है; वे जो कुछ भी कहते हैं वह मेरे अनुभव से मेल खाता है और मैं इससे सहमत हूँ। तुम्हारी वर्तमान समस्याओं के मूल कारण का उनका ब्यौरा सर्वथा सही है और इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है – सिवाय मेरे अधूरे पत्र में मैं जो साधना के भौतिक चेतना में उतर आने की बात कर रहा था, और वह भी वे जो कह रहे हैं उससे विसंगत नहीं है अपितु उसका परिपूरक है। इस कथन में भी वे सर्वथा उचित हैं कि इन भारी आक्रमणों का कारण भी तुम्हारा साधना को सच्चाई के साथ लेना, और, कहा जा सकता है, 'प्रकाश के राज्य' के द्वारों के समीप पहुँचना ही था। ऐसा उन ताकतों को सदा ही प्रचण्ड क्रोधावेश से भर देता है और वे साधक को पीछे मोड़ने के लिए अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगा देती हैं या उसके लिए हर संभव अवसर काम में लेती हैं, और संभव हुआ तो, अपने सुझावों, अत्यंत उग्र प्रभावों के द्वारा तथा इस प्रकार की परिस्थितियों में अधिकाधिक उठने वाली हर प्रकार की घटनाओं को अपने निहित प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाने के द्वारा उसे पूर्णतः पथ से हटा देने का प्रयास करती हैं ताकि वह द्वारों तक न पहुँच पाए। मैंने अनेक बार इन ताकतों की ओर संकेत करते हुए तुम्हें लिखा है, परंतु इस बात पर मैंने बहुत अधिक बल नहीं दिया क्योंकि उन अधिकांश लोगों की तरह जिनकी बुद्धि आधुनिक यूरोपीय शिक्षा के द्वारा तर्कप्रधान हो गई है, तुम्हारा भी इसमें विश्वास करने का, या कम-से-कम, इस ज्ञान को कोई महत्त्व प्रदान करने का कोई रुख नहीं था। इन दिनों लोग हर चीज की व्याख्या या उसका स्पष्टीकरण अपनी अज्ञ तर्क-बुद्धि, अपने सतही अनुभव और बाह्य घटनाओं में ढूँढ़ते हैं। वे गुप्त या प्रच्छन्न ताकतों और आंतरिक कारणों को नहीं देखते जो कि पारंपरिक भारतीय एवं यौगिक ज्ञान में सुपरिचित और दृष्टिगोचर थे। निःसंदेह, ये ताकतें अपने होने का कारण स्वयं साधक में, उसकी चेतना के अज्ञानमय भागों मैं और उन ताकतों के सुझावों और प्रभाव के प्रति उसकी स्वीकृति में ही पाती हैं; अन्यथा वे क्रिया ही नहीं कर सकती थीं या कम-से-कम किसी सफलता के साथ क्रिया नहीं कर सकती थीं। तुम्हारे मामले में, निम्नतर प्राणिक अहं की तुम्हारी चरम संवेदनशीलता ही उन ताकतों को सहारा प्रदान करने की मुख्य कारण रही है और अब भी तुम्हारे रूढ़ मतों अथवा पूर्वाग्रहों, पूर्वनिर्णयों, आदतन प्रतिक्रियाओं, निजी पसंदों, पुराने विचारों और संबंधों से चिपकाव वाली भौतिक चेतना और उसके जिद्दी संदेह को, और साथ ही इन सब चीजों को उच्चतर प्रकाश की अवरोधकारी और विरोधी दीवार के रूप में बनाए रखना ही उनका आश्रय बना है। भौतिक मन की इस क्रियाशीलता को ही लोग बुद्धि तथा तर्क-बुद्धि कहते हैं जबकि यह तो केवल मानसिक आदतों के घेरे में मशीन का चक्कर काटना है और यह उस सच्ची और मुक्त बुद्धि, उच्चतर बुद्धि से सर्वथा भिन्न है जो कि प्रबोधन या ज्ञान में समर्थ है और उससे भी कहीं अधिक उच्चतर आध्यात्मिक प्रकाश या आंतरात्मिक चेतना की उस अंतर्दृष्टि और सूक्ष्म विचार में समर्थ है जो तत्क्षण सच्चा और उचित क्या है उसे देख लेता है और जो गलत और मिथ्या है उससे उसका भेद कर लेता है। जब भी तुम एक अच्छी स्थिति में थे तब यह अंतर्दृष्टि सतत् ही तुम्हारे साथ थी, विशेषकर जब कभी तुममें भक्ति प्रबल हो जाती थी। जब साधक उन मानसिक और उच्चतर प्राणिक क्षेत्रों को छोड़कर, जिन पर कि वह सबसे पहले भगवान् की ओर मुड़ा था, भौतिक चेतना में उतरता है तो ये विरोधी चीजें बड़ी प्रबल और चिपकने वाली हो जाती हैं, और चूंकि उसकी अधिक सहायक अवस्थाएँ और अनुभूतियाँ पर्दे के पीछे चली जाती हैं और इसका भान भी उसे कदाचित् ही रहता है कि वे उसे कभी थीं भी, तो उस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि कृष्णप्रेम ने कहा और मैंने भी उस पर बल दिया है, तब केवल एक ही चीज है, वह है चिपके रहना अर्थात् पथ को दृढ़ता से पकड़े रहना। यदि एक बार साधक इन शक्तियों के गुप्त प्रस्तावों को, भले ही वे कितने भी सत्य सदृश क्यों न प्रतीत होते हों, मानने से इंकार करने का संकल्प प्राप्त कर सके और उसे बनाए रख सके तो यह स्थिति त्वरित रूप से या क्रमशः क्षीण होने लगती है और इसे पार किये जाने के बाद ये बंद हो जाएगी। जैसा कि कृष्णप्रेम ने और मैंने तुम्हें बताया है कि योग को त्याग देना कोई समाधान नहीं है; और यह करने में तुम सफल नहीं हो सकते और यही तुम्हारा मन भी तुम्हें तब बताता है जब वह शुद्ध होता है। संघर्ष से राहत के लिए आश्रम से कुछ समय के लिए बाहर जाना एक दूसरी बात है। हालाँकि, मैं नहीं समझता कि रमण आश्रम में निवास करना मन की कुछ शांति लौटाने के अतिरिक्त अंततोगत्वा अधिक कुछ सहायक सिद्ध होगा; रमण महर्षि एक महान् योगी हैं और अपने ही मार्ग में उनकी अनुभूति बहुत ऊँची है; परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह कोई ऐसा मार्ग है जिसका तुम उतना सफलतापूर्वक अनुसरण कर सको जितना कि अवश्य ही तुम भक्तिमार्ग का कर सकते हो यदि तुम उससे दृढ़तया चिपके रहो, और फिर अपना खुद का मार्ग खो देने और एक भिन्न प्रकृति के लिए उचित मार्ग का अनुसरण न कर पाने के कारण तुम्हारा दो तिपाइयों के बीच से गिरने का खतरा रहेगा।
"जहाँ तक बंगाल की बात है, स्थितियाँ निश्चय ही बहुत खराब हैं; हिंदुओं की स्थिति वहाँ भयंकर है और दिल्ली में अंतरिम सुविधाजनक गठबंधन होने के बावजूद वे बदतर भी हो सकती हैं। परंतु इसका हम पर निराशाजनक या अतिशय प्रभाव नहीं होना चाहिये। बंगाल में कम-से-कम दो करोड़ हिन्दू हैं और उनका सफाया नहीं किया जा सकता – यहाँ तक कि नरसंहार के वैज्ञानिक तरीकों से लैस हिटलर भी यहूदियों का सफाया नहीं कर सका जो कि अपने-आप को खूब जीवंत दिखा रहे हैं; और, जहाँ तक हिन्दू संस्कृति की बात है, वह कोई इतनी कमजोर और लसलसी या नरम चीज नहीं है जो आसानी से खत्म की जा सके; वह कम-से-कम कोई पाँच हजार सालों से चली आ रही है तथा और भी बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी और उसने इतनी शक्ति संग्रहीत कर ली है कि वह बची रह सकती है। जो कुछ हो रहा है वह मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने इसका तभी पूर्वानुमान कर लिया था जब मैं बंगाल में था और ऐसी स्थितियों की आशंका और लगभग उसकी अवश्यंभाविता के लिए और उसके लिए अपने-आप को तैयार करने के लिये मैंने लोगों को चेताया था। उस समय किसी ने भी मेरी कही बातों को कोई महत्त्व नहीं दिया यद्यपि जब बाद में समस्या शुरू हुई तब कुछ लोगों ने याद किया और स्वीकार किया कि मैं सही था; केवल सी. आर. दास को ही भारी शंकाएँ थीं और जब वे पांडिचेरी आए तब उन्होंने मुझे बताया भी कि वे नहीं चाहते कि जब तक वह खतरनाक समस्या निपट नहीं जाती है तब तक ब्रिटिश को जाना चाहिये। परंतु जो कुछ हो रहा है उससे मैं हतोत्साहित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ और सैकड़ों बार अनुभव भी किया है कि जो भगवान् का एक यंत्र है उसके लिए घोरतम अंधकार के परे भगवान् के विजय का प्रकाश मौजूद है। संसार में किसी भी चीज के घटित होने के लिए - मैं व्यक्तिगत चीजों की बात नहीं कर रहा - मेरा ऐसा कोई भी प्रबल और सुस्थिर संकल्प नहीं रहा जो कि विलंब, पराजय या फिर विध्वंस के बावजूद भी अंततः संसिद्ध न हुआ हो । एक समय था जब हिटलर सभी जगह विजयी था और यह निश्चित प्रतीत होता था कि असुर का काला जुआ (दमनकारी शासन) संपूर्ण संसार पर थोप दिया जाएगा; परंतु अब कहाँ है हिटलर और कहाँ है उसका राज? बर्लिन और न्यूरंबर्ग में मानव इतिहास के उस भयावह अध्याय का अंत इंगित हुआ था। अन्य कालिमाओं ने मानवजाति को ढक देने या फिर यहाँ तक कि उसे निगल जाने का संकट प्रस्तुत किया, परंतु जिस प्रकार पूर्वदुःस्वप्न का अंत हुआ वैसे ही उनका भी अंत होगा।"*
हमें यह याद रखना होगा कि हमारे अंदर भी इसी प्रकार के विद्रोही भाग चुपचाप दबे पड़े रहते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है तभी अपना सिर उठा लेते हैं। और तब वे अपनी सुविधानुसार नीति, धर्म और शास्त्र का सहारा लेकर ऊपर से दिखने में इतने सुंदर-सुंदर तर्क देते हैं कि कोई भी उनके धोखे में आ सकता है। इसीलिए यह बात अत्यंत महत्त्व की है कि हमारे सोचने समझने के तरीकों के स्थान पर, हमारी अपनी इच्छाओं-कामनाओं-लालसाओं आदि के स्थान पर श्रीमाँ के तौर तरीकों को और उन्हीं की इच्छा को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तभी जीवन में सच्चा परिवर्तन आ सकता है। और जब व्यक्ति अपना सभी कुछ श्रीमाँ के हाथों में सौंप देता है तभी स्वयं उसका और उसके सगे संबंधियों का सच्चा कल्याण हो सकता है।
--------------------------------------
* योगी श्रीकृष्णप्रेम, पृष्ठ ३९-४४
यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति स्वयं भी गर्त में गिरा होता है और जो उसके संपर्क में होते हैं उन्हें भी अपने प्रभाव से गर्न में ही धकेलता है। श्रीमाँ के संबंध से अलग हमारे अपने जितने भी निजी संबंध हैं उन्हें यदि हमने श्रीमाँ को समर्पित नहीं किया है तो वे सभी जंजीरें हैं जो हमें बाँधे रखती हैं और परमात्मा की ओर जाने से रोकती हैं। इसीलिये श्रीमाताजी के प्रति समर्पण और उनकी सेवा के भाव के साथ आरंभ तो हजारों लोग करते हैं, परंतु चूँकि मार्ग में ये सारे ही भटकाव जाल-घात लगाए रहते हैं, इस कारण वास्तव में पहुँचता कोई-कोई ही है। जब तक हमारे अंदर परोपकारिता या दूसरों की भलाई करने के विचार आते हैं तब तक तो हम अभी भ्रमित ही हैं। क्योंकि किसी की भी भलाई करने का एकमात्र सच्चा तरीका है अपने-आप को भगवान् को सौंप देना क्योंकि सच्चे रूप में वे ही जानते हैं कि किस व्यक्ति की किस चीज में भलाई है। अतः नियम एक ही है कि परिवार, देश, धर्म, कर्तव्य, कृतज्ञता, योग्यता आदि कोई भी चीज यदि आत्मा के यंत्र न बन सकें तो उसकी जंजीरों के समान हो जाते हैं। ये आत्मा के यंत्र तभी बनेंगे जब हम अपने-आप को श्रीमाँ के हाथों में सौंप देंगे। हालाँकि व्यवहार में यह कर पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे प्राण और शरीर के अपने-अपने बँधे-बँधाए ढरें होते हैं जिन्हें वे सहज ही छोड़ना नहीं चाहते। परंतु फिर भी कम-से-कम अपने हृदय और अपनी बुद्धि को तो हम श्रीमाँ से संलग्न कर ही सकते हैं। तब धीरे-धीरे आगे का रास्ता बैठने लगता है। श्रीअरविन्द बारंबार हमें याद दिलाते हैं कि सामान्यतया नैतिकता को, सात्त्विकता आदि को आध्यात्मिकता समझ लिया जाता है। जबकि आध्यात्मिकता से उनका कोई संबंध नहीं है। अधिक-से- अधिक वे तो केवल मानव को पाशविकता से निकाल कर मनुष्य बनाने में सहायक होते हैं। परंतु केवल गुरु के प्रति समर्पण और उनमें अपनी संपूर्ण प्रकृति का उत्सर्ग ही मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जा सकता है।
अर्जुन उवाच
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ।
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ।। ३७।।
३७. अर्जुन ने कहाः हे कृष्ण! जो श्रद्धापूर्वक योग को अपनाता है किन्तु मन आदि को वश में न कर सकने के कारण योग से विचलित मन वाला मनुष्य योग में सिद्धि को न प्राप्त कर के किस गति को प्राप्त होता है?
कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।। ३८।।
३८. हे महाबाहो ! क्या ब्रह्मप्राप्ति के मार्ग में मोहग्रस्त हुआ, स्थित न रहने के कारण (इस जीवन और ब्रह्म-चेतना) दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाने पर छिन्न-भिन्न हुए बादल के समान नष्ट तो नहीं हो जाता?
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः ।
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।। ३९।।
३९. हे कृष्ण। मेरे इस संशय को निःशेष रूप में निवृत्त कर दो। क्योंकि आप से भिन्न कोई दूसरा नहीं है जो इस संशय की निवृत्ति कर सके।
श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गतिं तात गच्छति ।। ४० ।।
४०. श्रीभगवान् ने कहाः हे पार्थ! उसका न इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है क्योंकि हे प्रिय! कल्याणकारी कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त होता।
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्नष्टोऽभिजायते ।। ४१।।
४१. योगभ्रष्ट मनुष्य पुण्य कर्म करनेवालों को जो लोक प्राप्त होते हैं उन्हें प्राप्त कर के और उनमें बहुत वर्षों तक निवास कर के पवित्र और श्रीसंपन्न व्यक्तियों के घर में जन्म ग्रहण करता है।
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ।। ४२।।
४२. अथवा वह बुद्धिमान् योगियों के ही कुल में जन्म ग्रहण कर सकता है; ऐसा जो जन्म है यह इस पृथ्वी लोक में निःसंदेह अति दुर्लभ है।
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।। ४३।।
४३. हे कुरुनंदन अर्जुन ! (इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में) वह उस पूर्व देह में प्राप्त की हुई बुद्धि के साथ संयोग को प्राप्त करता है और तदनंतर पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिये पहले की अपेक्षा अधिक परिश्रम से प्रयत्न करता है।
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।। ४४।।
४४. पूर्वजन्म के अभ्यास के प्रताप से ही अवश रूप से या प्रबल रूप से आगे ले जाया जाता है; योग के ज्ञान का जिज्ञासु भी वेद उपनिषदादि के शाब्दिक ज्ञान से परे पहुँच जाता है।
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः ।
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ।। ४५।।
४५. और परिश्रम के साथ अभ्यास करते हुए, समस्त पापों से शुद्ध होकर, अनेक जन्मों के परिश्रम से अपने आप को सिद्ध किया हुआ योगी परम् गति को प्राप्त होता है।
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।
कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ।। ४६।।
४६. योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है और कर्म करनेवाले व्यक्तियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है यह मेरा अभिमत है; इसलिये हे अर्जुन! योगी हो।
योगी वह है जो कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा अथवा चाहे जिस तरह से हो केवल आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान, शक्ति के लिये शक्ति या अन्य किसी चीज के लिए वह चीज नहीं चाहता, अपितु केवल भगवान् के साथ ऐक्य ही खोजता है और उसे प्राप्त करता है; उसी ऐक्य में सभी कुछ समाहित रहता है और उसी में सब कुछ अपने रूप से ऊपर उठकर परम भागवत् अर्थ को प्राप्त हो जाता है। परन्तु योगियों में भी भक्त ही सबसे श्रेष्ठ होता है।
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।। ४७।।
४७. समस्त योगियों में भी जो योगी अपने संपूर्ण अंतरात्मा से मेरे को समर्पण करता है, मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा रखता है, उसे मैं अपने साथ सबसे अधिक योगयुक्त हुआ मानता हूँ।
इसमें यह तो स्पष्ट ही है कि गीता सभी चीजों का निरूपण करने के बाद भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताती है और सभी कुछ की पराकाष्ठा या परिणति ब्रह्म में नहीं अपितु भगवान् की भक्ति, उनसे प्रेम में बतलाती है। जब अर्जुन अपने कर्मों से होने वाले फल को सोचकर भयवश सकुचा रहा था तब उसे आश्वस्त करते हुए भगवान् ने उसे एक बड़ा भारी वचन दिया कि इस योग मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास नष्ट नहीं होता, न ही कोई प्रत्यागमन ही होता है, और इस धर्म का थोड़ा-सा अनुष्ठान भी महान् भय से मुक्त कर देता है। परन्तु जैसा कि अर्जुन की प्रकृति का चित्रण करते हुए श्रीअरविन्द कहते हैं कि वह बुद्धि के द्वारा चालित नहीं अपितु अपने इंद्रिय-संवेदनों के द्वारा चालित व्यक्ति था और अपनी बाहरी प्रकृति में ही निवास करता था इसीलिए कदाचित् वह उस वचन का मर्म पूरी तरह समझ नहीं पाया अन्यथा अब जो उसने प्रश्न किया बह संभवतः उठता ही नहीं। क्योंकि वह जानता था कि मन को वश में करने का भारी काम उसके लिये संभव नहीं है, इसलिये योग उसके लिये संभव ही नहीं है। इसलिए वह पुनः उसी प्रश्न को दोहराता है जिसके प्रत्युत्तर में भगवान् उसे समझाते हैं कि ज्ञान, तपस्या, कर्म आदि तो केवल साधन मात्र हैं, साध्य तो परमात्मा हैं। योगी उनसे ऐक्य साधित करने का प्रयास करता है इसलिए वह श्रेष्ठ होता है और योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक योगयुक्त वही है जो 'मेरे में प्रेम और श्रद्धा रखता है और मेरे प्रति समर्पित है'। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान् के समीप चला जाता है उसे उनसे प्रेम न हो, ऐसा हो नहीं सकता। यदि व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो परंतु भगवान् के प्रति भक्ति न हो तब तो इसका अर्थ है कि वास्तव में उसके अन्दर उनके स्वरूप का सच्चा ज्ञान अभी तक नहीं आया है। और यदि व्यक्ति के अन्दर भक्ति हो पर उनके सत्स्वरूप का ज्ञान न हो तो इसका अर्थ है कि उसके अन्दर सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान दोनों साथ-साथ चलते हैं और फिर इनके साथ-ही-साथ सच्चा कर्म भी आता ही है। यदि व्यक्ति के अन्दर ज्ञान और भक्ति हो पर वह भगवान् के लिए कर्म न करता हो तो इसका अर्थ है कि न तो उसे उनके स्वरूप का ज्ञान है और न ही उनके प्रति भक्ति है। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि जिसके प्रति हमारा प्रेम हो, जिसके प्रति हमारी भक्ति हो उसके लिए हम कर्म न करें। इसलिए सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति और सच्चा कर्म साथ-साथ ही चलते हैं और परस्पर एक-दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और पूर्ण बनाते हैं।
यही गीता के प्रथम छः अध्यायों का अंतिम वचन है और इसी में शेष सब का बीज निहित है, उस सबका बीज निहित है जो अभी कहना बाकी है और जो कहीं भी पूर्णतया नहीं कहा गया है; क्योंकि वह सदा कुछ अंश में रहस्य और गुह्य ही बना रहता 3 - 44 आध्यात्मिक रहस्य, दिव्य रहस्य।
[अब हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि शुरू के इन छः अध्यायों में जिस मूल प्रश्न को लेकर गीता का उपक्रम हुआ, उसका समाधान कहाँ तक हुआ है।। यहाँ पुनः यह उल्लेख कर देना उपयोगी होगा कि स्वयं उस प्रश्न में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए संपूर्ण विश्व के स्वरूप का और सामान्य जीवन के स्थान पर आध्यात्मिक जीवन की प्रतिष्ठा का विचार आवश्यक होता। उपस्थित प्रश्न का विचार व्यावहारिक या नैतिक रूप से या बौद्धिक दृष्टि से अथवा आदर्शवाद की दृष्टि से या इन सब दृष्टियों से एक साथ ही किया जा सकता था; और यह वस्तुतः कठिनाई को हल करने की हमारी आधुनिक पद्धति होती...। गीता यह अनुभव करती है कि इस दृष्टिकोण से कोई परम् निरपेक्ष समाधान नहीं, अपितु एक तात्कालिक व्यावहारिक समाधान ही हो सकता है, और अर्जुन के सामने उस काल के उच्चतम आदर्श के अनुसार ऐसा ही एक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने पर, जिसे उसकी चित्त-वृत्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं है और वास्तव में उसका स्वीकार करना अभिप्रेत भी नहीं है, गीता उस प्रश्न के समाधान के लिए एक सर्वथा दूसरे ही दृष्टिकोण की ओर और सर्वथा दूसरे ही हल की ओर बढ़ती है।
गीता का समाधान है हमारी प्राकृत सत्ता और साधारण मन से ऊपर, हमारे बौद्धिक और नैतिक भ्रमजालों के ऊपर उस दूसरी चेतना में उठना जहाँ सत्ता का एक दूसरा ही विधान प्रभावी है और इसीलिए वहाँ हमारे कर्म के लिए दूसरा ही दृष्टिकोण है; जहाँ व्यक्तिगत कामना और व्यक्तिगत भावावेग उसे संचालित नहीं करते; जहाँ द्वन्द्व दूर हो जाते हैं; जहाँ कर्म हमारे निजी नहीं रह जाते और इसलिए जहाँ व्यक्तिगत पाप और पुण्य के बोध को अतिक्रम कर दिया जाता है; जहाँ विराट् नैयक्तिक भागवत् सत्ता हमारे द्वारा जगत् में अपने हेतु को क्रियान्वित करती है; जहाँ हम स्वयं एक दिव्य नवजन्म के द्वारा उसी सत् के सत्, उसी चित् के चित्, उसी शक्ति की शक्ति, उसी आनन्द के आनन्द हो जाते हैं और तब, अपनी इस निम्न प्रकृति में नहीं रहने से, हमारे अपने करने के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते, कोई अपना निजी हेतु नहीं रह जाता और यदि हम कर्म करते भी हैं, - और यही एकमात्र वास्तविक समस्या और कठिनाई रह जाती है, - तो केवल भागवत् कर्म ही करते हैं, वे कर्म जिनमें बाह्य प्रकृति कर्म का कारण या प्रेरक नहीं, केवल एक अप्रतिरोधी उपकरण मात्र होती है; क्योंकि प्रेरक शक्ति तो हमारे ऊपर हमारे कर्मों के अधीश्वर की इच्छा में रहती है। और यही हमें सच्चे समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि यह हमारी सत्ता के वास्तविक सत्य तक लौटता है और अपनी सत्ता के वास्तविक सत्य के अनुसार जीना ही स्पष्टतया जीवन के प्रश्नों का संपूर्णतः सर्वोत्कृष्ट और एकमात्र समाधान है...। हम उस महत् सत्य को उसमें निवास कर के ही जान सकते हैं, अर्थात् योग के द्वारा मानसिक अनुभव के परे आध्यात्मिक अनुभव में पहुँचने पर ही जान सकते हैं। क्योंकि, अंततः योग से हमारा अभिप्राय ही यही है कि तब तक आध्यात्मिक अनुभूति में जीवन व्यतीत करना जब तक हम मानसभाव से छूट कर आत्मभाव में प्रतिष्ठित न हो जाएँ, जब तक वर्तमान प्रकृति के दोषों से मुक्त होकर अपनी यथार्थ और भागवत् सत्ता में पूर्ण रूप से रहने न लग जाएँ।
हमारी सत्ता के केन्द्र का यह ऊर्ध्व स्थानांतरण और परिणामतः हमारे संपूर्ण अस्तित्व तथा चेतना का रूपान्तरण जिसके फलस्वरूप अपनी बाह्य प्रतीति में कर्म के वैसे का वैसा ही बने रहने पर भी उसके संपूर्ण आंतरिक भाव और हेतु का परिवर्तन हो जाना ही गीता के कर्मयोग का सारतत्त्व है। अपनी सत्ता को रूपान्तरित करो, आत्मा में नवजन्म लो और उस नवीन जन्म से उस कर्म में लगो जिसके लिए तुम्हारी अंतःस्थित आत्मा ने तुम्हें नियुक्त किया है, यही गीता के संदेश का मर्म कहा जा सकता है। अथवा दूसरी तरह से, अधिक गंभीर और अधिक आध्यात्मिक आशय के साथ यों कहें कि, जो कर्म तुम्हें यहाँ करना पड़ता है उसे अपने आन्तर आध्यात्मिक नवजन्म का साधन बना लो, अपने दिव्य जन्म का साधन बना लो, और फिर दिव्य होकर, भगवान् के उपकरण बनकर लोकसंग्रह के लिए दिव्य कर्म करो। अतः यहाँ दो बातें हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से निर्धारित करना और समझना होगा, एक है इस परिवर्तन, इस ऊर्ध्व स्थानांतरण का मार्ग, यह दिव्य नवजन्म, और दूसरी बात है कार्य का स्वभाव या यों कहें वह मनोभाव जिसमें कि वह कार्य निष्पादित करना है...।
हम इस आधार से आरंभ करते हैं कि मनुष्य का वर्तमान आंतर जीवन जो लगभग पूरी तरह उसकी प्राण-प्रकृति और शरीर-प्रकृति पर निर्भर है और जो मानसिक शक्ति की सीमित क्रीड़ा के द्वारा कुछ ही ऊपर उठा रहता है, वही उसका संपूर्ण संभाव्य जीवन नहीं है, न यह उसके वर्तमान वास्तविक जीवन का ही सब कुछ है। उसके अन्दर एक आत्मा छिपी हुई है और उसको वर्तमान प्रकृति या तो उस आत्मा का केवल बाह्य रूप है या उसकी क्रिया-शक्ति का एक आंशिक फल। गीता सर्वत्र इस क्रिया-शक्ति की वास्तविकता को स्वीकार करती प्रतीत होती है, कहीं भी ऐसा नहीं मालूम होता कि उसने चरमपंथी वेदांतियों का यह कठोर मत स्वीकार किया हो कि यह सत्ता केवल एक प्रतीति या आभास है, यह एक ऐसा मत है जो समस्त कार्यों और कर्म के मूल पर ही कुठाराघात करता है। गीता ने अपनी दार्शनिक विवेचना में इस पहलू को जिस रूप में सामने रखा है (यह दूसरे रूप में भी रखा जा सकता था) वह यही है कि उसने सांख्यों का प्रकृति-पुरुष-भेद मान लिया है - पुरुष अर्थात् वह ज्ञान-शक्ति जो जानती, धारण करती और पदार्थ मात्र को अनुप्राणित करती है और प्रकृति अर्थात् वह क्रिया-शक्ति जो कर्म करती और नानाविध उपकरणों, माध्यमों और प्रक्रियाओं को जुटाती रहती है। भेद इतना ही है कि गीता ने सांख्यों के मुक्त अक्षर पुरुष को ग्रहण तो किया है, किन्तु उसे वेदान्त की भाषा में 'एक' अक्षर सर्वव्यापक आत्मा या ब्रह्म कहा है, और दूसरे प्रकृतिबद्ध पुरुष से उसका पार्थक्य दिखाया है। यह प्रकृतिबद्ध पुरुष ही हमारा क्षर कर्मशील पुरुष है, यही बहुपुरुष है जो समस्त वस्तुओं में है और जो विभिन्नता और व्यक्तित्व का आधार है। परन्तु तब प्रकृति का कर्म क्या है?
'गीता सर्वत्र इस क्रिया-शक्ति की वास्तविकता को स्वीकार करती प्रतीत होती है, कहीं भी ऐसा नहीं मालूम होता कि उसने चरमपंथी वेदांतियों का यह कठोर मत स्वीकार किया हो कि यह सत्ता केवल एक प्रतीति या आभास है, यह एक ऐसा मत है जो समस्त कार्यों और कर्म के मूल पर ही कुठाराघात करता है।' वेदान्तियों का कहना है कि 'ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या', जगत् मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, स्वप्न की तरह है, परछाई मात्र है, लाठी में साँप को देखने की भाँति है, आदि-आदि। परन्तु गीता ऐसा नहीं मानती। गीता इसे आत्मा की ही क्रिया मानती है, हालाँकि वह क्रिया और अभिव्यक्ति सीमित है, आंशिक है। और वह इस जगत् को मिथ्या नहीं बल्कि सत्य मानती है, परंतु सत्य हमारी इंद्रियों के अर्थ में नहीं, अपितु एक गहरे अर्थ में, आत्मा की दृष्टि से। पर वास्तव में इस जगत् का स्वरूप कैसा है इसका बोध तो ज्यों-ज्यों हमारी चेतना विकसित होती जाती है त्यों-त्यों अधिक विशाल और गहन होता जाता है। गीता यदि वेदान्तियों के चरमपंथी मत को ही स्वीकार करती तब तो वह अर्जुन को युद्ध का आदेश देकर स्वयं अपनी ही शिक्षा का खंडन कर रही होती। यदि गीता इस जगत् को मिथ्या ही मानती तब तो इसके लिए इस सब युद्ध आदि की बात करना तो बिल्कुल असंगत होता।
यह प्रक्रिया की शक्ति, प्रकृति, है जो कि तीनों गुणों की एक दूसरे पर क्रिया-रूप क्रीड़ा है। और, माध्यम क्या है? यह प्रकृति के उपकरणों के क्रम-विकास से सृष्ट जीवन की जटिल प्रणाली है और जैसे-जैसे ये उपकरण प्रकृति की क्रिया में जीव की अनुभूति के अन्दर प्रतिभासित होते हैं वैसे-वैसे हम इन्हें क्रमशः बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रियाँ और पंचमहाभूत कह सकते हैं, और ये पंचमहाभूत ही प्रकृति के रूपों के आधार हैं। ये सब यांत्रिक हैं, ये प्रकृति का एक जटिल यंत्र है; और आधुनिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि ये सब-के-सब जड़ प्राकृतिक शक्ति में समाए हुए हैं और प्रकृतिस्थ जीव जैसे-जैसे प्रत्येक यंत्र के ऊर्ध्वगामी विकास के द्वारा अपने-आपके विषय में सचेतन होता जाता है वैसे-वैसे ये प्रकृति में प्रकट होते हैं, किन्तु जिस क्रम से हम इन्हें ऊपर गिना आये हैं, उससे इनके प्रकटीकरण का क्रम उल्टा होता है, अर्थात् पहले जड़ सृष्टि प्रकट होती है, तब इन्द्रिय-समूह, उसके बाद क्रम से मन और बुद्धि और अंत में आत्मचेतना। तर्क-शक्ति या बुद्धि जो पहले प्रकृति के कार्यों में ही लगी रहती है, बाद में इन कार्यों के यथार्थ स्वरूप को खोज निकाल सकती है, उन कार्यों को तीनों गुणों के मात्र खेल के रूप में देख सकती है जिसमें कि जीव फँसा हुआ है, वह जीव को तथा त्रिगुण के इन कार्यों को अलग-अलग देख सकती है; तब जीव को यह अवसर मिलता है कि वह इस बंधन से अपने-आपको छुड़ा ले और अपने मूल मुक्त स्वरूप और अक्षर सत्ता में लौट आये। तब वेदान्तिक परिभाषा में जीव आत्मा को, सत्ता को, देखता है; प्रकृति के उपकरणों और कार्यों से, उसके अभिव्यक्त रूपों से अपना तादात्म्य बन्द कर देता है; अपनी यथार्थ आत्मा के साथ, अपने सत्स्वरूप के साथ तदात्म होता और अपनी स्वतः सिद्ध अक्षर आत्मसत्ता को फिर से पा लेता है। गीता के अनुसार इसी आत्मस्थिति से वह मुक्त भाव से तथा अपनी सत्ता के ईश्वररूप से अपनी अभिव्यक्ति के कर्म का आश्रय बन सकता है।
लगभग सभी साधनाओं में यह बात तो सर्वमान्य ही है कि आरंभ में व्यक्ति मन, प्राण और शरीर की क्रियाओं में ही रमा रहता है और उनसे बँधा हुआ होता है इसलिए जब वह इनसे कुछ मुक्त होता है तब उसे यह आभास होता है कि इन सबसे परे किसी अन्य चीज का भी अस्तित्व है। गीता की गति का यह पहला सोपान है। अठारहवें अध्याय के ६२वें श्लोक में भगवान् अर्जुन को पहले तो सर्वभाव से उन ईश्वर की शरण में जाने के लिये कहते हैं 'तमेव शरणं गच्छ' जो कि समस्त भूतों के हृदय में अवस्थित हैं और अपनी माया के द्वारा यन्त्र पर आरूढ़ के समान समस्त भूतों को घुमाते रहते हैं। परंतु ऐसा कहने के बाद भगवान् उसे स्वयं अपने ही पास आने का उपदेश करते हैं 'मन्मना भव मद्भक्तो', 'मामेकं शरणं व्रज'। श्रीअरविन्द यहाँ कहते हैं कि इस पार्थिव सृष्टि के निर्माण में जिस क्रम से चेतना का घनीकरण हुआ, क्रमविकास में उससे उल्टे क्रम में उनका विकास होता है। और इसलिए क्रमविकास के अंदर जड़भौतिक तत्त्व पहले आता है और प्राण उसके बाद। केवल मन के आने के बाद ही प्राणिक प्रकृति भौतिक पर कुछ अंकुश लगाना आरंभ करती है। इसीलिए मन पर नियंत्रण करने के लिए उच्चतर मन की, उसके बाद अधिमन की और उसके बाद अतिमन की आवश्यकता होती है। जितना ही हम चेतना के उच्चतर शिखरों पर आरोहण करते जाएँगे उतना ही अधिक नियंत्रण निचले भागों पर साधित हो पाएगा। यह एक सामान्य तरीका है।
प्रश्न : इस प्रक्रिया शक्ति में प्रकृति के माध्यम क्या हैं? क्या मन, प्राण, बुद्धि आदि प्रकृति के माध्यम हैं जिनके द्वारा वह अपनी क्रिया करती है?
उत्तर : ये सब आत्मा के तत्त्व नहीं हैं, प्रकृति की चीजें हैं। यहाँ तक कि बुद्धि भी आत्मा का तत्त्व नहीं है। प्रकृति ही विवेक करती है, वही अपने-आप को ऊपर उठाती है। हम कह सकते हैं कि परमात्मा के दो तत्त्व हैं - सत् और चित्। चित् अर्थात् चेतना जिसके दो अंग हैं - चित् और तपस् अर्थात् चेतना और ऊर्जा। यही प्रकृति का आधिपत्य करती है। इसमें आत्मतत्त्व तो केवल साक्षीस्वरूप होता है। वास्तविक कर्तृ तो चेतना है और यही प्रकृति का माध्यम है। ऊपर की चेतना को पराप्रकृति कह देते हैं और इसे निम्न प्रकृति कहते हैं। यद्यपि आत्मतत्त्व ही सभी कुछ का सच्चा कर्ता है तो भी बाह्य प्रतीति में आत्मतत्त्व केवल साक्षित्व करता है और क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है। वास्तव में प्रकृति केवल वही करती है जो आत्मतत्त्व चाहे। उसकी इच्छा के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं करती। वह तो उसी की अभिव्यक्ति करने के लिए, उसी के सत्य और उसकी अंतर्वस्तु को सामने लाने के लिए क्रमशः अधिकाधिक उन्नत रूपों का निर्माण करती है ताकि किसी प्रकार उस आत्मतत्त्व को अभिव्यक्त कर सके। यह तो ऐसा ही है मानो प्रकृति केवल उस आत्मतत्त्व के अनंतविध रूपों को ही प्रतिबिंबित कर रही हो। परन्तु चूंकि हमारा प्रकृति से तादात्म्य होता है इसलिए यह सत्य हमारे लिए विस्मृत हो जाता है और हम अवश रूप से प्रकृति की क्रियाकलाप में ही विचरण करते रहते हैं। जबकि हमारा एक भाग - चैत्य - ऐसा है जो इस भूल-भुलैया में नहीं फँसता। वह पराप्रकृति का ही अंश होता है।
केवल उन मनोवैज्ञानिक तत्त्वों को देखते हुए, जिन पर ये दार्शनिक भेद आधारित हैं, - दर्शनशास्त्र अस्तित्व के मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक तथ्यों के तथा ऐसी किसी चरम यथार्थता (यदि ऐसी कोई हो) के साथ इनके संबंध के सारमर्म को हमारे अपने लिए बौद्धिक रूप से स्पष्ट करने का एक तरीका मात्र है, - हम यह कह सकते हैं कि हम दो तरह के जीवन बिता सकते हैं, एक है अपनी सक्रिय प्रकृति के कार्यों में लीन जीव का जीवन, जिसमें जीव अपने मनोवैज्ञानिक और बाह्य उपकरणों के साथ तदाकार, उनसे सीमित, अपने व्यक्तित्व से बँधा, प्रकृति के अधीन होता है; और दूसरा है आत्मा का जीवन जो इन सब चीजों से श्रेष्ठ, विशाल, नैयक्तिक, विश्वव्यापी, मुक्त, अपरिमित, लोकोत्तर है और अपने असीम समत्व से अपनी प्राकृत सत्ता और कर्म को धारण करता पर अपनी मुक्त स्थिति और अनन्त सत्ता से इनके परे रहता है। हम चाहें तो अपनी वर्तमान प्राकृत सत्ता में रह सकते हैं और चाहें तो अपनी महत्तर आत्मसत्ता में रह सकते हैं। यही वह पहला महान् भेद है जिस पर गीता का कर्मयोग प्रतिष्ठित है।
क्षर और अक्षर ये दो भेद हैं। जब व्यक्ति प्रकृति से तदात्म होता है तब वह क्षर पुरुष कहलाता है जिसमें सब बदलता रहता है। अक्षर भाव में रहने पर वह शाश्वत्, अमर, निर्विकल्प, निराकार, निर्लेप और असीम है। अक्षर भाव में कर्म नहीं किया जा सकता। कर्म करने के लिए तो क्षर भाव अपनाना होता है। इनसे ऊपर का भाव है पुरुषोत्तम भाव जो इन दोनों से परे है और बिना बद्ध हुए वह इन दोनों ही भावों में सफलतापूर्वक क्रिया कर सकता है। पुरुषोत्तम की इच्छानुसार ही सभी कुछ होता है। प्रकृति तो वही करती है जो वह चाहता है। इसीलिए भगवान् कहते हैं कि “मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ"। प्रकृति तो उनकी सेवक होती है जो उनकी प्रसन्नता के निमित्त सभी कुछ की व्यवस्था करती है। इसलिए क्षर-अक्षर का विभाग दिखलाकर और इनकी अपनी-अपनी सीमितता दिखलाकर अंत में गीता इनसे परे जाने का उपदेश करती है क्योंकि इन दोनों भावों में तो कर्मयोग संभव ही नहीं है चूंकि क्षर भाव में तो व्यक्ति प्रकृति की क्रिया में लिप्त रहता है और उससे बद्ध रहता है, और अक्षर भाव में कर्म संभव ही नहीं हैं। इसलिए सच्चा कर्मयोग तो तभी संभव है जब व्यक्ति इनसे परे चला जाए। क्षर भाव में सच्चे कर्म करने की समस्या को देखते हुए ही शंकराचार्य आदि का मत रहा है कि केवल अज्ञानी जन ही कर्म करते हैं। जो ज्ञानी है वह तो अक्षर ब्रहा की शांति में स्थित हो जाता है और कर्मों से मुक्त हो जाता है। परंतु गीता इसका समाधान पुरुषोत्तम तत्त्व का निरूपण कर के करती है।
प्रश्न : इस चर्चा से यह समझ आता है कि व्यक्ति या तो प्रकृतिबद्ध इस निम्नतर जीवन में लिप्स रह सकता है या फिर वह चेतना में ऊपर उठकर प्रकृति से परे मुक्ततर भाव में भी जा सकता है जहाँ वह श्रेष्ठ तरीके से जी सकता है और सफलतापूर्वक कर्म कर सकता है। परंतु इस चयन की हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी है कि हम यह चुनाव कर सकें कि इनमें से हमें कौनसा जीवन जीना है?
उत्तर : यदि व्यक्ति अपने-आप को अहं से तदात्म करता है तब तो चयन का कोई अधिकार नहीं होता। और यदि व्यक्ति अपने-आप को वह समझता है जो वास्तव में अपने अंतर में वह है, तब चयन की पूरा स्वतंत्रता होती है। यह विकल्प चुनने का अधिकार वास्तव में जो आप हैं उसे, अर्थात् आपकी वास्तविक सत्ता को है। अहं को तो यह सत्ता केवल अपने उपयोग में लेती है। यह सारा विधान उसी सत्ता का है। वही मन, प्राण और शरीर को धारण करती है और इनके द्वारा वह अपना जो काम करवाना चाहती है उसी के अनुसार इनमें इच्छाएँ, कामनाएँ, उत्प्रेरणाएँ आदि जैसी आवश्यक होती हैं वैसी ही पैदा कर देती है। जब तक उसे लगता है कि बाहरी प्रकृति से तादात्म्य आवश्यक है तब तक वह तादात्म्य बनाए रखती है और जब उसे लगता है कि यह आवश्यक नहीं है तब वह उससे तादात्म्य हटा लेती है। इसलिए व्यक्ति अपने अहं की अपेक्षा जितना ही अपनी इस सच्ची सत्ता से जुड़ा होता है उतना ही उसका मूल्य है। और जब वह इससे जुड़ा होता है तब वह सभी निम्न प्रभावों से ऊपर उठ जाता है और महत् कर्म कर सकता है। इसके बिना तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता। इस विषय में योगी श्रीकृष्णप्रेम कहते हैं कि, "जिस हद तक हम अपने उच्चतम और अंतरतम 'आत्मस्वरूप' के द्वारा क्रिया करते हैं, उस हद तक हम मुक्त होते हैं।
जिस हद तक हम अपने-आप को आत्मा के साथ तदात्म कर देते हैं, उतना ही हम 'उनकी' सृष्टि-क्रिया में मुक्त रूप से भागीदार हो रहे होते हैं और तब न कोई बाध्यताएँ रह जाती हैं न कोई सीमाएँ क्योंकि तब हम ही इसमें संकल्प कर रहे होते हैं या हर हाल में हम ही 'उनके' साथ इच्छा कर रहे होते हैं।
जिस हद तक हम अपने-आप को शरीर और मन (स्मरण रहे, यह भी प्रकृति है) से तदात्म करते हैं उस हद तक हम बद्ध हैं क्योंकि हम अपने-आप को उन घटनाओं की श्रृंखला से बाँध रहे होते हैं जो कि आत्मा की अर्थात् 'उनकी' और हमारी इच्छा से श्रृंखलागत रूप से घटित होती हैं।
तो तुम देखो कि आध्यात्मिक रूप से पूर्ण मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र होता है जबकि जो देहादि से पूरी तरह से तदात्म होता है वह पूर्णतः 'बद्ध' होता है। वास्तविकता में, हालाँकि, मुझे नहीं लगता कि आत्मा कभी भी दूसरे (अर्थात् जड़) के साथ पूर्णतः एकात्म होती है। जहाँ तक आत्मा पर जड़तत्त्व हावी होता है वहाँ तक वह बद्ध प्रतीत होती है और जहाँ तक जड़तत्त्व पर आत्मा का प्रभुत्व होता है वहाँ तक वह मुक्त प्रतीत होता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मनुष्य में आत्मा पूर्ण रूप से अधीन या पूरी तरह से बद्ध होती है। सदा ही उसका 'एक अंश' मुक्त और अपनी निज प्रकृति में बना रहता है। और यहीं सामान्य मनुष्य का प्रवेश होता है, वह मनुष्य जो न तो निरा पशु है और न ही अभी तक अत्यधिक विकसित आत्मा है।
....विशुद्ध आत्मा शुद्ध स्वतंत्रता है परंतु चूँकि विशुद्ध आत्मा का अर्थ निष्क्रिय आत्मा है तो यह एक अमूर्त विषय है। शुद्ध जड़तत्त्व निरा बंधन है परंतु शुद्ध जड़तत्त्व जैसी कोई चीज नहीं होती। वह भी एक अमूर्त विषय है। अनुभव में सदा ही आत्मा और जड़तत्त्व संलग्न रहते हैं इसलिए अनुभव के साथ स्वतंत्रता और बंधन का मिश्रण लगा रहता है। जो अनुभव से परे है वह समस्त वर्गीकरण से परे है।" (योगी श्रीकृष्णप्रेम, पृष्ठ १७५-७६)
इसलिए अब सारा प्रश्न और सारा तरीका यही है कि अंतरात्मा को अपनी वर्तमान प्राकृत सत्ता की सीमाओं से मुक्त किया जाए। हमारे स्वाभाविक जीवन में प्रथम तथ्य जो हम पर हावी रहता है वह है जड़ प्रकृति के रूपों, पदार्थों के बाह्य स्पर्शों के प्रति हमारी अधीनता। ये (रूप और स्पर्श) अपने आप को इन्द्रियों के द्वारा हमारे प्राण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और प्राण तुरंत इन्द्रियों के द्वारा इन्हें पकड़ने के लिए और इनसे व्यवहार करने के लिए दौड़ पड़ता है, इनकी कामना करता है, इनसे आसक्त होता है और फल की इच्छा करता है। अपने सभी आंतरिक संवेदनों, सब प्रतिक्रियाओं, भावावेगों, बोध करने, चिंतन करने और अनुभव करने के अपने अभ्यस्त तरीकों में सभी में मन इन्द्रियों की इसी क्रिया का अनुगमन करता है; मन के बहकावे में आकर बुद्धि भी अपने-आपको इन्द्रियों के इस जीवन को सौंप देती है, यह जीवन जिसमें आंतरिक सत्ता वस्तुओं के बाह्य रूपों में ही फंसी रहती है और क्षण भर के लिए भी वास्तव में उनसे ऊपर नहीं उठ सकती या हमारे ऊपर होने वाली इसकी क्रिया के घेरे से अथवा हमारे अन्दर होनेवाले उसके मनोवैज्ञानिक परिणामों और प्रतिक्रियाओं के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकती। यह उनसे परे नहीं जा सकती क्योंकि अहंकार का तत्त्व विद्यमान है, जिसके द्वारा बुद्धि हमारे मन, इच्छा, इन्द्रियसमूह और शरीर पर होनेवाले प्रकृति के संपूर्ण कार्य को अन्यान्य मनों, स्नायविक संघटनों और शरीरों पर होनेवाले कार्यों से पृथक् बोध करती है; और हमारे लिए हमारे जीवन का उतना ही अर्थ रह जाता है जितना हमारे अहंकार पर प्रकृति का असर पड़ता है और हमारा अहंकार उसके स्पर्शों का प्रत्युत्तर देता है, इसके सिवाय हम और कुछ नहीं जानते, हमें लगता है कि हम और कुछ हैं ही नहीं; स्वयं आत्मा भी मानो मन, इच्छा, भावावेगमय और स्नायवीय अभिग्रहण (reception) और प्रतिक्रिया का ही कोई पृथक् पुंज लगती है। हम अपने अहंकार को विशाल बना सकते हैं, अपने-आपका कुल, जाति, वर्ग, देश, राष्ट्र, मनुष्यजाति तक के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं; परन्तु फिर भी इन सब छद्मरूपों में अहंकार ही हमारे सब कर्मों की जड़ बना रहता है, केवल बाह्य पदार्थों के साथ अपने इन विस्तृततर व्यवहारों के द्वारा उसे अपनी पृथक् सत्ता की एक बृहत्तर संतुष्टि प्राप्त होती है।
इस स्थिति में भी हमारे अन्दर प्राकृत सत्ता की इच्छा ही काम करती है जो अपने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं को तृप्त करने के लिए ही बाह्य जगत् के स्पर्शों को ग्रहण करती है, और इस प्रकार विषयों को ग्रहण करनेवाला संकल्प सदा ही कर्म और कर्मफल के प्रति कामना, आवेश और आसक्तिमय होता है; यह हमारी प्रकृति की ही इच्छा होती है; इसे हम अपनी निजी इच्छा कहते हैं, पर हमारा अहंभावापन्न व्यक्तित्व तो प्रकृति की ही एक रचना है, यह हमारी मुक्त आत्मा, हमारी स्वाधीन सत्ता नहीं है और न हो ही सकता है। यह सारा प्रकृति के गुणों का कर्म है। यह कर्म तामसिक हो सकता है और तब हमारा व्यक्तित्व जड़वत्, वस्तुओं की यांत्रिक धारा के वशवर्ती और उसी से संतुष्ट, किसी अधिक स्वाधीन कर्म को और प्रभुत्व के किसी प्रबल प्रयास को करने में सर्वथा असमर्थ होता है। अथवा यह कर्म राजसिक हो सकता है और तब हमारा व्यक्तित्व अशांत और क्रियाशील होता है, जो अपने-आपको प्रकृति पर लादना और उससे अपनी आवश्यकताएँ और इच्छाएँ पूरी करवाना चाहता है, पर यह नहीं देख पाता कि उसका यह प्रभुत्व का आभास भी एक दासत्व ही है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएँ वे ही हैं जो प्रकृति की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ हैं, और जब तक हम उनके वश में हैं तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। अथवा यह कर्म सात्त्विक हो सकता है और तब हमारा व्यक्तित्व प्रबुद्ध होता है, जो बुद्धि के द्वारा अपना जीवन बिताने और किसी शुभ, सत्य या सुन्दर के अभीष्ट आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है; पर अब भी यह बुद्धि प्रकृति के रूपों के ही वश में होती है और ये आदर्श हमारे अपने ही व्यक्तित्व के परिवर्तनशील भाव होते हैं जिनमें अंततोगत्वा कोई सुनिश्चित नियम नहीं मिलता न कोई स्थायी संतोष ही मिलता है। यहाँ भी हम परिवर्तन के पहिये पर ही घूमते रहते हैं और उस शक्ति के अधीन रहते हैं जो हमारे अन्दर और इस सबके अन्दर है और जो अहंकार के द्वारा इस तरह चक्कर लगवाती है, पर हम स्वयं वह शक्ति नहीं होते न उसके साथ हमारा योग या मेल ही होता है। यहाँ भी कोई मुक्तावस्था या यथार्थ प्रभुत्व नहीं होता।
फिर भी मुक्तावस्था संभव है। उसके लिए पहले हमें अपनी इन्द्रियों पर होनेवाली बाह्य संसार की क्रियाओं से अलग हटकर अपने-आप में आना होगा; अर्थात् हमें अंतर्मुख होकर रहना होगा और इन्द्रियाँ जो अपने बाह्य विषयों की ओर स्वभावतः दौड़ पड़ती हैं, उन्हें रोके रखने में समर्थ होना होगा। इन्द्रियों को अपने वश में रखना और इन्द्रियाँ जिन चीजों के लिए तरसा करती हैं उनके बिना सुखपूर्वक रहने में समर्थ होना, सच्चे आध्यात्मिक जीवन की पहली शर्त है; जब ऐसा हो जाता है केवल तभी हम यह अनुभव करने लगते हैं कि हमारे अन्दर कोई आत्मा है जो बाह्य स्पर्शों से उत्पन्न होनेवाले मन के विकारों से सर्वथा भिन्न वस्तु है, वह आत्मा जो अपनी गंभीरतर सत्ता में स्वयंभू, अक्षर, शांत, आत्मवान्, भव्य, स्थिर, गंभीर और महान् है, स्वयं ही अपना प्रभु है और बाह्य प्रकृति की व्यग्रता भरी दौड़-धूप से सर्वथा अलिप्त है। परन्तु यह तब तक नहीं हो सकता जब तक हम कामना के वश में हैं। क्योंकि हमारे समस्त बाह्य जीवन का मूल तत्त्व यह कामना ही है जो अपने आप को इन्द्रियगत जीवन से तुष्ट करती है और आवेगों (षड्रिपुओं) की क्रीड़ा में ही अपना पूरा लेखा-जोखा पाती है।
प्राण का यह प्रभाव मन और शरीर दोनों में प्रवेश करता है और इसके प्रभाव से कदाचित् ही कोई बच पाता है। प्राण के आवेगों में जब व्यक्ति फँस जाता है तब उसकी कामनाएँ और अधिक विशाल रूप ले लेती हैं जिसके प्रभाव से व्यक्ति में गरीबों की सेवा, दुनिया में अपना नाम कमाने आदि की बड़ी भारी महत्त्वाकांक्षाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। और सामान्यतया ऐसे व्यक्तियों को महान् की संज्ञा दे दी जाती है जो दुनिया में कोई अतिविशाल कर्म करते हैं। परंतु कामना के वशीभूत होकर कर्म करने में और भागवत् संकल्प की अभिव्यक्ति के लिए कर्म करने में भारी अंतर होता है। इसलिए हम श्रीरामकृष्णजी की तुलना किसी ऐसे व्यक्तित्व से नहीं कर सकते जिसने कामना के वशीभूत हो महत् कार्य सिद्ध किये हों। और यह कामना व्यक्ति के सभी भागों में प्रवेश कर के उनमें अपना प्रभाव छोड़ देती है।
इसलिए हमें कामना से छुटकारा पाना होगा, और प्राकृत सत्ता की इस प्रवृत्ति के नष्ट होने पर हमारे मनोविकार, जो कामना के भावावेगमय परिणाम होते हैं, अपने-आप ही शान्त हो जाएँगे; क्योंकि लाभ और हानि से, सफलता और असफलता से, प्रिय और अप्रिय स्पर्शों से जो सुख-दुःख हुआ करते हैं, जो इन मनोविकारों का सत्कार करते हैं, हमारी आत्माओं में से निकल जाएँगे। तब एक प्रशान्त समता प्राप्त होगी। और चूँकि हमें अब भी इस जगत् में रहना और कर्म करना होता है और हमारा स्वभाव कर्म के फल की आकांक्षा करने वाला है, अतः हमें इस स्वभाव को बदलना होगा और फल की आसक्ति को छोड़ कर कर्म करना होगा, अन्यथा कामना और उसके सारे परिणाम पूर्ववत् बने रहेंगे। परन्तु हममें कर्म के कर्त्ता का जो स्वभाव है उसे हम कैसे बदल सकते हैं? कर्मों को अहंकार और व्यक्तित्व से अलग कर के, विवेक-बुद्धि से यह देखकर कि यह सब कुछ केवल प्रकृति के गुणों का ही खेल है, और अपनी आत्मा को इस खेल से विलग कर के, सबसे पहले उसे प्रकृति के कर्मों की साक्षी बना के तथा उन कार्यों को उस शक्ति के भरोसे छोड़कर जो वास्तव में उनके पीछे है; यह शक्ति प्रकृति के अन्दर रहनेवाली ऐसी कोई चीज है जो हमसे महत्तर है, यह हमारा व्यक्तित्व नहीं अपितु वह शक्ति है जो विश्व की स्वामिनी है। परन्तु मन इस सब की अनुमति नहीं देता; क्योंकि उसका स्वभाव इन्द्रियों के पीछे भागना और बुद्धि और इच्छाशक्ति को अपने साथ घसीट ले जाना है। इसलिए हमें मन को स्थिर करना सीखना होगा। हमें वह निरपेक्ष शान्ति और स्थिरता प्राप्त करनी होगी जिसमें पहुँच कर हम उस अंतःस्थित स्थिर, अचल, आनन्दमय आत्मा को जान सकें जो सदा बाह्य पदार्थों के स्पर्शों से अप्रभावित, अक्षुब्ध रहती है, जो अपने-आप में पूर्ण रहती है और वहीं अपनी शाश्वत परितृप्ति लाभ करती है...।
प्रश्न : कामना का मूल कारण क्या है?
उत्तर : जैसे ही अहंकार आता है वैसे ही एक पृथक् अस्तित्व का बोध आ जाता है। और एक पृथक् अस्तित्व होते ही व्यक्ति को स्वयं को सुरक्षित बनाए रखने का, चीजों को हस्तगत करने का, अपने से पृथक् सत्ता के साथ व्यवहार का बोध उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में तो सभी कुछ एक ही है इसलिए पृथक्ता का बोध आते ही अपूर्णता का बोध भी आ जाता है। और इस अपूर्णता को पूरा करने के लिए कामना आ जाती है। बिना कामना के जड़-तत्त्व में जीवन विकसित ही नहीं हो सकता था। यदि पशुओं में कोई कामना न हो तो वे कोई क्रिया ही नहीं करेंगे। इसलिए भय और कामना इन दो चीजों को प्रकृति में रोपित किया गया। परंतु ये ही चीजें जो विकास की प्रक्रिया में किसी समय आवश्यक थीं, उनकी उपयोगिता खत्म होने पर अवरोध भी बन जाती हैं। इसलिए जो चीज वर्तमान में हमारी सहायक है वही कालांतर में हमारे लिए बाधक भी बन सकती है। गीता भी अपनी सारी शिक्षा को इस ओर विकसित कर रही है कि साधक सभी कुछ में से होकर सभी धर्मों को त्याग देने की स्थिति तक आ जाए। परंतु अक्षर पुरुष के संपर्क में आने की जो बात गीता कह रही है वह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम है। परंतु इससे पार्थिव अभिव्यक्ति में कोई विशेष लाभ नहीं होता। इससे तो व्यक्ति केवल निम्न प्रकृति के प्रभाव से कुछ सुरक्षित बना रह सकता है। परंतु इस स्थिति में कोई वास्तविक प्रभुत्व नहीं है। उसके लिए तो पुरुषोत्तम भाव में ही जाना होगा। यही गीता का रहस्य है।
जब यह आत्मा हमारे अंदर प्रकाशित होती है, जब हमें इसकी शान्ति और नीरवता का अनुभव होता है, तब हम इसमें संवर्द्धित हो सकते हैं; प्रकृति में निमज्जित निम्नतर अवस्था में हमारे अंतःपुरुष की स्थिति को स्थानांतरित कर हम उसे आत्मा में पुनः प्रतिष्ठित कर सकते हैं। हम ऐसा उन वस्तुओं की शक्ति से कर सकते हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं- स्थिरता, समता, निर्विकार नैर्व्यक्तिकता। क्योंकि ज्यों-ज्यों हम इन चीजों में विकसित होते हैं, उन्हें अपनी पूर्णता तक पहुँचाते हैं और अपनी सारी प्रकृति को इनके अधीन कर देते हैं, त्यों-त्यों हम इस स्थिर, सम, निर्विकार, नैयक्तिक, सर्वव्यापक आत्मा के स्वरूप में विकसित होते जाते हैं। हमारी इन्द्रियाँ उसी नीरवता में जा पहुँचती हैं और जगत् के स्पर्शों को परम् प्रशान्ति के साथ ग्रहण करती हैं: और हमारा मन उसी नीरवता को प्राप्त होकर शान्त, विराट् साक्षी बन जाता है: और हमारा अहंकार इसी नैयक्तिक सत्ता में विलीन हो जाता है। तब हम सभी चीजें उसी आत्मा में देखते हैं जो कि हम अपने आप में बन चुके होते हैं; और हम सबमें इस आत्मा को देखते हैं; हम सब भूतों के साथ उनको आत्मसत्ता में एकीभूत हो जाते हैं। इस अहंभावशून्य शान्ति और नैयक्तिकता में रहते हुए हम जो कर्म करते हैं वे हमारे अपने कर्म नहीं रह जाते, वे अब अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें किसी भी प्रकार से न तो बाँध सकते हैं न कोई पीड़ा ही पहुँचा सकते हैं। प्रकृति और उसके गुण अब भी अपने कर्म का जाल बुना करते हैं, पर उनसे हमारी दुःख-रहित स्वतःसिद्ध शान्ति भंग नहीं होती। सब कुछ उसी एक सम विराट् ब्रहा में समर्पित होता है।
यहाँ यह एक वर्णन है और कुछ-एक व्यक्ति इस मार्ग से जा सकते हैं। परंतु ये सभी स्थितियाँ मनोवैज्ञानिक रूप से या फिर आत्मपरक रूप से तो संभव हैं परंतु जब तक अचेतन और निश्चेतन स्तरों का रूपांतर नहीं हो जाता, तब तक व्यावहारिक रूप से ये संभव नहीं हैं। जैसा कि गीता में 'जितः सर्गः' आदि अवस्थाओं का वर्णन आता है कि ऐसा योगी संसार को जीत लेता है या फिर वह निर्विकल्प समाधि अवस्था में चला जाता है जहाँ ये निम्न प्रभाव विचलित नहीं करते, परंतु यह तो बहुत ही अधिक श्रम कर के सभी चीजों का निषेध कर के प्राप्त की गई स्थितियाँ हैं। इनमें प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने की भव्यता नहीं होती। सहज रूप से प्रकृति पर पूर्ण प्रभुत्व की तो बात ही अलग है। इसी बिंदु को श्रीअरविन्द अब सामने लाएँगे।
परन्तु यहाँ दो कठिनाइयाँ हैं। एक यह कि इस शान्त अक्षर आत्मा और प्रकृति के कर्म में एक अंतर्विरोध प्रतीत होता है...। प्रकृति कोई पृथक् सत्ता नहीं अपितु परमेश्वर की ही शक्ति है जो विश्वरचना में प्रवृत्त होती है। परन्तु परमेश्वर यदि केवल यही अक्षर पुरुष हैं और व्यष्टि-पुरुष केवल कोई ऐसी चीज है जो उसमें से निकलकर उस शक्ति के साथ इस सृष्टि में आया है, तो जिस क्षण व्यष्टि-पुरुष लौटकर आत्मा में स्थित होगा उसी क्षण सारी सृष्टिक्रिया बन्द हो जायेगी, और पीछे छोड़ेगी केवल परम् एकता और परम् निस्तब्धता। दूसरे, यदि अब भी किसी अचिंत्य रूप से कर्म जारी रहें तो भी आत्मा जब सब पदार्थों के लिए सम है तब कर्म हों या न हों और हों तो चाहे जैसे हों, इसका कोई महत्त्व नहीं। ऐसी अवस्था में यह भयंकर और सर्वनाशी प्रकार का कर्म क्यों, यह रथ, यह युद्ध, यह योद्धा, यह दिव्य सारथी किसलिए?
भगवान् अर्जुन को अक्षर ब्रह्म में जाने का उपदेश करते हैं। परंतु यदि कर्मों के होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता और जब व्यक्ति निर्लिप्त होकर अक्षर ब्रह्म की स्थिति में पहुँच जाता है और उसका कर्मों से कोई लेना-देना ही नहीं रहता तब फिर अर्जुन को किसी छोटे-मोटे कर्म में ही नहीं बल्कि इस घोर युद्ध कर्म में नियोजित करना तो असंगत बात होती। इसलिए गीता इस समस्या को लेकर यहीं नहीं रुक सकती।
गीता इसका उत्तर यह बतलाकर देती है कि परमेश्वर अक्षर पुरुष से भी महान् हैं, अधिक व्यापक हैं, वे साथ-साथ यह पुरुष भी हैं और प्रकृति में होनेवाले कर्म के अधीश्वर भी। परन्तु वे अक्षर ब्रह्म की सनातनी शांति, समता, कर्म और व्यष्टिभाव में स्थित रहते हुए प्रकृति के कर्मों का संचालन करते हैं। हम कह सकते हैं कि यही उनकी सत्ता की वह स्थिति है, जिसमें से वे कर्म संचालन करते हैं, और जैसे-जैसे हम इस स्थिति में संवर्द्धित होते हैं वैसे-वैसे हम उन्हीं की सत्ता और दिव्य कर्मों की स्थिति को प्राप्त होते हैं। इसी स्थिति से वे अपनी सत्ता की प्रकृतिगत इच्छा और शक्ति के रूप में निकल आते हैं, अपने-आपको सब भूतों में प्रकट करते हैं, जगत् में मनुष्यरूप में जन्म लेते हैं, सब मनुष्यों के हृदयों में निवास करते हैं, अवताररूप से अपने-आपको अभिव्यक्त करते हैं (यही मनुष्य के अन्दर उनका दिव्य जन्म है); और मनुष्य ज्यों-ज्यों उनकी सत्ता में संवर्द्धित होता है, त्यों-त्यों वह भी इस दिव्य जन्म को प्राप्त होता है। इन्हीं प्रभु के लिये जो हमारे कर्मों के अधीश्वर हैं, यज्ञ के तौर पर कर्म करने होंगे और अपने-आपको आत्मस्वरूप में उन्नत करते हुए हमें अपनी सत्ता में उनके साथ एकत्व लाभ करना होगा और अपने व्यष्टिभाव को इस तरह देखना होगा कि यह उन्हीं का प्रकृति में आंशिक प्राकट्य है। सत्ता में उनके साथ ऐक्य लाभ करने से हम जगत् के सब प्राणियों के साथ एक हो जाते हैं और दिव्य कर्म करने लगते हैं, अपने कर्म के तौर पर नहीं अपितु लोक संरक्षण और लोकसंग्रह के लिये हमारे द्वारा होनेवाली उन्हीं की क्रिया के तौर पर।
इसलिए कर्मों की समस्या का समाधान गीता पुरुषोत्तम तत्त्व के द्वारा करती है जिन्हें कि किसी व्यक्तिगत लाभ की कोई आवश्यकता नहीं परंतु फिर भी लोकसंग्रह के लिए वे कर्मों में रत रहते हैं। और व्यक्ति ज्यों-ज्यों इस स्थिति की ओर अग्रसर होता है त्यों-त्यों वह दिव्य रूप से कर्म करने लगता है। तब सारे संसार पर उसका सहज अधिकार हो जाता है क्योंकि वह प्रभु की चेतना में रहते हुए क्रिया करता है।
यही करने योग्य मूलभूत चीज है और एक बार इसे संपन्न करते ही अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत होने वाली सब कठिनाइयाँ लुप्त हो जाएँगी। प्रश्न तब हमारे वैयक्तिक कर्म का नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व जिससे बनता है वह तो केवल इस लौकिक जीवन से संबंध रखनेवाली और इसलिए गौण चीज रह जाती है, तब फिर जगत् में हमारे द्वारा भगवदिच्छा के कार्यान्वित होने का प्रश्न ही रह जाता है। उसे समझने के लिए यह जानना होगा कि ये परमेश्वर स्वयं क्या हैं और प्रकृति के अन्दर इनका क्या स्वरूप है, प्रकृति की कर्मपरंपरा क्या है और उसका लक्ष्य क्या है और प्रकृतिस्थ पुरुष और इन परमेश्वर के बीच आंतरिक संबंध कैसा है, इसे समझने के लिए ज्ञानयुक्त भक्ति ही आधार है। इन्हीं बातों का स्पष्टीकरण गीता के शेष अध्यायों का विषय है।
इस प्रकार छठा अध्याय 'आत्मसंयमयोग' समाप्त होता है।
सातवाँ अध्याय
I. दो प्रकृतियाँ
गीता के प्रथम छः अध्याय एक प्रकार से इसकी शिक्षा का मानो एक प्रारम्भिक खण्ड तैयार करते हैं; शेष सभी बचे बारह अध्याय इस खण्ड में आए अधूरे तत्त्वों का ही विशद निरूपण हैं, जो तत्त्व इस प्रथम खण्ड में मूलभावों के पीछे केवल संकेत रूप से ही आए हैं परंतु अपने-आप में अत्यंत महत्त्व के हैं अतः इन्हें बाकी के दो षटकों में विशद निरूपण के लिए रख छोड़ा गया है।... इसमें बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिन्हें जो आगे आएगा उसके द्वारा डाले गए प्रकाश की सहायता के बिना ठीक तरह नहीं समझा जा सकता...
स्वयं अर्जुन ही, यदि श्रीगुरु अपना उपदेश यहीं समाप्त कर देते तो, यह आपत्ति कर सकता था किः "आपने कामना और आसक्ति के नाश, समत्व, इन्द्रियों पर विजय और मन को शांत स्थिर करने, निष्काम और निरहंकार कर्मों, कर्मों के यज्ञ, बाह्य संन्यास से आंतर संन्यास के श्रेष्ठत्व के बारे में बहुत कुछ कहा, और इन सब बातों को मैं बौद्धिक रूप से तो समझता हूँ, भले ही ये आचरण में लाने में मुझे कितनी भी कठिन प्रतीत क्यों न होती हों, परन्तु आपने व्यक्ति के कर्म में रत रहते हुए भी गुणों से ऊपर उठने की बात भी कही है, और मुझे यह नहीं बताया कि गुण कैसे कार्य करते हैं, और जब तक मैं यह नहीं जान लेता, तब तक गुणों का पता लगाना और उनसे ऊपर उठना मेरे लिए कठिन होगा। इसके अतिरिक्त आपने भक्ति को योग के प्रधानतम अंग के रूप में बताया है, फिर भी आपने कर्म और ज्ञान के बारे में तो बहुत कुछ कहा है, पर भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा और कहा भी है तो बहुत थोड़ा। और, फिर यह भक्ति, जो सबसे महत् चीज है, किसे अर्पण की जानी है? अवश्य ही शान्त निर्गुण ब्रह्म को नहीं, अपितु आप ईश्वर को। इसलिए अब आप मुझे यह बताइए कि आप क्या हैं, कौन हैं, क्योंकि जैसे भक्ति आत्मज्ञान से भी महत्तर है वैसे ही आप उस अक्षर ब्रह्म से बड़े हैं जो क्षर प्रकृति और कर्ममय संसार से उसी तरह बड़ा है जैसे ज्ञान कर्म से बड़ा है। इन तीनों चीजों में परस्पर क्या संबंध है? कर्म, ज्ञान और भगवत् प्रेम में परस्पर क्या संबंध है? प्रकृतिस्थ पुरुष, अक्षर पुरुष और वह जो सबके अव्यय आत्मा होने के साथ-साथ समस्त ज्ञान, भक्ति और कर्म के प्रभु, परमेश्वर हैं, जो यहाँ इस महायुद्ध और भीषण रक्तपात में मेरे साथ हैं, इस घोर भयानक कर्म के रथ में मेरे सारथी हैं, इन तीनों में परस्पर क्या संबंध है?" इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शेष गीता लिखी गई है, और समस्या के एक पूर्ण बौद्धिक समाधान में इन सभी को अविलंब लेकर हल करना होगा। परंतु वास्तविक साधना के क्षेत्र में व्यक्ति को क्रमशः ही आगे बढ़ना होता है और बहुत-सी बातों को, यहाँ तक कि बड़ी-से-बड़ी बातों को भी समय आने पर अपने-आप उठने और आध्यात्मिक अनुभव से अपने-आप ही सुलझने के लिए छोड़े रखना पड़ता है। एक हद तक गीता अनुभव की इस रेखा का अनुसरण करती है और पहले कर्म और ज्ञान का एक प्रकार का एक विशाल प्राथमिक आधार निर्मित करती है जिसमें एक ऐसा तत्त्व निहित है जो भक्ति तक और महत्तर ज्ञान की ओर ले जाता है, परंतु अभी गीता वहाँ तक पहुँचती नहीं है। प्रथम छः अध्याय हमें यही आधार प्रस्तुत करते हैं।...
अधिकांश टीकाकार गीता के छठे अध्याय तक आते-आते इसकी शिक्षा की इतिश्री घोषित कर देते हैं। परन्तु श्रीअरविन्द कहते हैं कि प्रथम छः अध्यायों में तो गीता की शिक्षा के तत्त्व केवल संकेत रूप से ही आए हैं जिनका विशद निरूपण तो अभी किया जाना बाकी है। पहले छः अध्यायों में तो गीता अपनी शिक्षा का एक विशाल प्राथमिक आधार निर्मित करती है। सात से बारह तक के अगले छः अध्याय बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें भक्ति तत्त्व का तथा पूर्ण भगवत्ता का निरूपण होगा। हालाँकि इन अध्यायों में पुरुषोत्तम तत्त्व का स्पष्ट निरूपण तो नहीं हुआ है परंतु फिर भी विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन भगवान् के स्वरूप का वर्णन करते हुए 'त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः' आदि संज्ञाओं से उनका स्तवन करता है। यदि आम टीकाकारों के मतानुसार पहले छः अध्याय ही गीता की संपूर्ण शिक्षा का सार हों तब तो सच्चे कर्म आदि की गुत्थियों को सुलझाना तथा अन्य गंभीरतर रहस्यों को उद्घाटित करना तो बाकी ही रह जाता है। पुरुषोत्तम तत्त्व का निरूपण हुए बिना तो कर्म का कोई आधार ही नहीं रह जाता क्योंकि क्षर भाव में सच्चे कर्म संभव नहीं हैं, और अक्षर भाव में तो कर्म ही संभव नहीं हैं। तब फिर निष्काम कर्म तथा दिव्य कर्म की बात तो एक ऐसी असंगत बात हुई जिसका गीता उपदेश तो करती है परंतु जो व्यवहार में संभव नहीं है। वैसे ही, बिना पुरुषोत्तम तत्त्व का निरूपण हुए भक्ति का भी कोई अर्थ नहीं निकलता और भक्ति का निरूपण हुए बिना न तो ज्ञान ही अपनी सच्ची परिणति पाता है और न ही कर्मों का कोई सच्चा आधार प्राप्त होता है। इसलिए आगे आने वाले अध्यायों के बिना गीता के पहले छः अध्यायों में निहित संकेतों का स्पष्टीकरण नहीं होता।
इन्हीं तत्त्वों का अब निरूपण करते हुए सबसे पहले महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या गुणों से परे होकर कोई कर्म संभव हैं, क्योंकि निम्न प्रकृति में तो सभी कर्म त्रिगुणमय होते हैं और जब तक ये गुण प्रभावी होते हैं तब तक सच्चा कर्म नहीं हो सकता। अब चूंकि प्रकृति ही क्रियाशक्ति है और उसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता तो क्या कोई उच्चतर प्रकृति भी है जिसकी क्रिया गुणों से परे हो क्योंकि यदि उच्चतर प्रकृति न हो तब तो अवतारों की क्रिया भी प्रकृति के गुणों के अधीन ही हुई, और ऐसे में तो दिव्य कर्म आदि की बातें तो बिल्कुल बेतुकी और अतर्कसम्मत हुईं जिनमें अपने आप में ही विरोधाभास है। इसीलिए गीता दो प्रकृतियों के बीच के भेद को प्रकट करती है जिसके निरूपण से ही कर्म की गुत्थी सुलझ सकती है। सात से बारह तक के अध्याय भगवान् की दिव्य प्रकृति, जगदंबा के स्वरूप का ही निरूपण हैं। उसी के लिए योग है, उसी के लिए भक्ति है, वही सभी कुछ का आधार है। विश्वरूप-दर्शन भी भगवान् की दिव्य प्रकृति का ही दर्शन है क्योंकि अपने आप में पुरुष का तो दर्शन होता नहीं, वह तो एक भाव है। दर्शन तो भगवान् की क्रियाशक्ति का ही होता है।
सातवें से बारहवें तक के अध्याय दिव्य पुरुष की प्रकृति का एक व्यापक तात्त्विक निरूपण प्रस्तुत करते हैं और उसके आधार पर ज्ञान और भक्ति को घनिष्ठ रूप से ठीक उसी प्रकार संबद्ध और समन्वित करते हैं जैसे कि गीता के प्रथम षटक् ने कर्म और ज्ञान को जोड़ा और समन्वित किया था। विश्वपुरुष-दर्शन, जो कि बीच में ग्यारहवें अध्याय में आया है, इस समन्वय को एक शक्तिशाली रूप प्रदान करता है और इसे कर्म और जीवन के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ देता है। इस प्रकार सब चीजें फिर से प्रभावशाली रूप से अर्जुन के मूल प्रश्न पर लायी जाती हैं जिसके चारों ओर यह व्याख्या घूमती व अपना चक्र पूरा करती है। बाद में गीता प्रकृति और पुरुष का भेद समझाकर गुणों के कार्य और त्रिगुणातीतता या निखैगुण्य की अवस्था के बारे में तथा निष्काम कर्मों की उस ज्ञान में परिसमाप्ति, जहाँ वह भक्ति के साथ एक हो जाता है, के बारे में अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करती है। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति में एकता साधित कर गीता उस परम् वचन की ओर मुड़ती है जो सब भूतों के महान् ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के संबंध में उसका परम् रहस्य है।
---------------
'प्रतीत होता है कि यहाँ हम कुछ अधिक स्पष्टतर क्षेत्र में आ गए हैं, और एक घनीभूत और अधिक सटीक अभिव्यक्ति हमारी पकड़ में आ रही है। परन्तु इस घनीभूतता के कारण ही हमें बराबर सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा जिससे कि कोई त्रुटि न हो जाए, और कहीं हम वास्तविक अर्थ को चूक न जाएँ। क्योंकि, यहाँ हम मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभूति की सुरक्षित भूमि पर स्थित होकर नहीं चल रहे हैं, अपितु यहाँ हमें आध्यात्मिक और प्रायः विश्वातीत सत्य के बौद्धिक विवरणों से व्यवहार करना होता है। तात्त्विक प्रतिपादन में सदा ही यह आशंका और अनिश्चितता बनी रहती है कि यह उस चीज को हमारी बुद्धि के समक्ष परिभाषित या निरूपित करने का प्रयास है जो वास्तव में असीम है; यह एक ऐसा प्रयास है जो करना तो पड़ता है पर जो कभी भी सर्वथा संतोषजनक, सर्वथा निर्णायक या आखिरी नहीं हो सकता। परम् आध्यात्मिक सत्य को जीया जा सकता है, उसका दर्शन किया जा सकता है, परंतु उसका वर्णन केवल अंशतः ही हो सकता है। उपनिषदों की गंभीरतर निरूपण पद्धति और भाषा ही जिसमें रूपक और प्रतीक का मुक्त प्रयोग है, जिसमें भाषा की अंतर्ज्ञानात्मक शैली के प्रयोग के कारण बौद्धिक अभिव्यक्ति की कठोर और सीमित कर देने वाली निश्चितता का बंधन तोड़ दिया गया है और शब्दों के गर्भित अर्थों को संकेतों की अबाध तरंग में बह निकलने दिया गया 3 - 37 (गंभीरतर आध्यात्मिक) क्षेत्रों में एकमात्र उचित निरूपण पद्धति और भाषा होती है। परन्तु गीता इस निरूपण शैली का सहारा नहीं ले सकती क्योंकि इसे बौद्धिक समस्या के समाधान के लिए रचा गया है, यह मन की एक ऐसी स्थिति को उत्तर देती है या उसे संतुष्ट करती है जिसमें तर्क-बुद्धि, जो कि ऐसी न्यायकर्ता है जिसके समक्ष हम अपने आवेगों और भावों की कलहों को समाधान हेतु प्रस्तुत करते हैं, स्वयं अपने आप के साथ संघर्षरत है और किसी समाधान पर पहुँचने में असमर्थ है। तर्क-बुद्धि को एक ऐसे सत्य की ओर ले जाना है जो उसके परे है, परंतु उसे वहाँ तक उसी के अपने साधन और अपनी ही रीति से ले जाना है। तर्क-बुद्धि के सामने आत्मानुभव का यदि कोई ऐसा समाधान रखा जाए जिसके तथ्यों के विषय में उसे स्वयं कुछ भी अनुभव न हो तो उसकी सत्यता पर उसे तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक उस समाधान के मूल में विद्यमान आत्मिक सत्यों का बौद्धिक निरूपण करके उसे सन्तुष्ट न कर दिया जाए।
गीता के इस द्वितीय खण्ड में हम निरूपण की शैली को अब तक की शैली की अपेक्षा अधिक संक्षिप्त' और सरल पाते हैं।
यह पादटिप्पणी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इसमें निहित सत्य बहुत ही गूढ़ है। इससे हमें इस बात का रहस्य पता चलता है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने वेदों और उपनिषदों की अभिव्यक्ति रूपकों और प्रतीकों के माध्यम से क्यों की? ऐसा नहीं था कि उनमें स्पष्ट बौद्धिक अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं थी, और न ही ऐसा था कि वे जानबूझकर उस सत्य को छिपाना चाह रहे हों। परंतु बात यह है कि उस सत्य को किसी अन्य तरीके से प्रकट किया जा ही नहीं सकता। और यदि उन सत्यों का बौद्धिक निरूपण किया जाए तो, पहले तो, उन सत्यों का सर्वांगीण स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा और, दूसरे, उनका भयंकर रूप से गलत अर्थ लगाये जाने और उनका दुरुपयोग होने की आशंका बन जाती है। परंतु चूंकि अर्जुन के प्रश्न मानसिक धरातल से ही उठ रहे हैं इसलिए उनके उत्तर मानसिक स्तर पर ही दिये जा सकते हैं। अपने वर्तमान गठन के अनुसार अर्जुन से बौद्धिक स्तर से ऊपर उठने की आशा नहीं की जा सकती और गहन आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए अभी वह तैयार ही नहीं है। परंतु जिन मूलभूत प्रश्नों को अर्जुन उठाता है उनका समाधान बौद्धिक स्तर पर संभव नहीं है। उनके समाधान के लिए जिस स्तर के सत्यों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता है उन्हें बौद्धिक स्तर पर लाने में अपने खतरे निहित हैं। परंतु गीता को तो इसी धरातल पर उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे क्योंकि यदि वह उन प्रश्नों को उन्हीं की भाषा में उत्तर न दे तो उसकी प्रासंगिकता ही नहीं रहेगी। पहले छः अध्यायों में गीता जिन मनोवैज्ञानिक सत्यों के विषय में चर्चा कर रही थी उन्हें हम कुछ हद तक तो अवश्य ही महसूस कर सकते हैं परंतु जिन विषयों में गीता अब प्रवेश करने जा रही है वे तो बहुत ही गहन आध्यात्मिक और विश्वातीत सत्य हैं। परंतु बौद्धिक रूप से निरूपण करने के कारण हम उन्हें सामान्य और सहज मान बैठने की भूल कर सकते हैं और अधिकांशतः लोग ऐसा करते ही हैं जबकि वास्तव में तो वे अत्यंत गूढ़ सत्य होते हैं। बौद्धिक भाषा में अब जो सत्य प्रकट किये जाएँगे वे अंतःप्रकाशमय (revelatory) सत्य हैं जो कि सामान्य अनुभूति से परे हैं। अंतःप्रकाशमय सत्यों को अपनी प्रामाणिकता के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। यदि अनुभव उन्हें सिद्ध नहीं करता तो अनुभव को संदिग्ध या अप्रामाणिक माना जाता है न कि उन अंतःप्रकाशमय सत्यों को। इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए हम श्रीअरविन्द के वेद विषयक लेख के ही कुछ अंश को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं, "साधारणतया आधुनिक युक्तिपूर्ण मन द्वारा, जो स्वयं अनुमान की तात्त्विक पद्धति द्वारा या निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अपने बौद्धिक निष्कर्षों तक पहुँचने का अभ्यस्त है, ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों के उत्कृष्ट सामान्य विचार, जो देखने में तात्त्विक प्रकृति के प्रतीत होते हैं, अवश्य ही सक्रिय तात्त्विक अनुमानों का परिणाम रहे हैं जो कि वेदों की आदिम रूप से कल्पनात्मक तथा संवेदनात्मक धार्मिक धारणाओं को उन्नत एवं बौद्धिक बनाने के प्रयास से उत्पन्न हुए थे। मैं इस मत को एक ऐसी भ्रान्ति मानता हूँ जो हमारी वर्तमान मानसिक प्रणालियों को वैदिक ऋषियों की सर्वथा भिन्न मानसिकता में आरोपित करके समझने के प्रयास के कारण उत्पन्न होती है। प्राचीन जगत् की उच्चतर मानसिक प्रणालियाँ बौद्धिक नहीं अपितु अंतर्बोधात्मक थीं। वे अत्यंत देदीप्यमान, अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत अस्पष्ट आंतरिक क्रियाएँ ही हमारे ज्ञान के विशालतम और सशक्ततम स्रोत हैं परंतु तार्किक बुद्धि के लिए इनका अर्थ अत्यंत अस्पष्ट और प्रामाणिकता संदेहास्पद है। अंतःप्रकाश (Revelation), अंतःप्रेरणा (Inspiration), अंतर्ज्ञान (Intuition), तथा अंतर्ज्ञानात्मक विवेक (Intuitive discrimination) प्राचीन अनुसंधान की प्रधान प्रणालियाँ थीं। आधुनिक मानव की तर्कशील बुद्धि के लिए अंतःप्रकाश एक मिथ्या कल्पना है, अंतःप्रेरणा विचारों और शब्दों का बौद्धिक रूप से केवल द्रुत चयन मात्र है, अंतर्ज्ञान तर्कसंगत बुद्धि की तीव्र और अस्पष्ट प्रक्रिया है और अंतर्ज्ञानात्मक विवेक अनुमान करने का उत्कृष्ट और आनंददायक तरीका है। किन्तु वैदिक बुद्धि के लिए वे प्रणालियाँ न केवल वास्तविक और सुपरिचित ही थीं अपितु प्रामाणिक प्रक्रियाएँ थीं; हमारे भारतीय प्राचीन लोग उन्हें सत्य तक पहुँचने के परमोच्च साधनों के रूप में मानते थे, और यदि केंट (Kant) की ही रीति का अनुगमन करते हुए कोई वैदिक ऋषि वेद की समीक्षा करता तो उसने प्राचीन शब्दों, दृष्टि, श्रुति, स्मृति, केतु के पीछे आधारभूत विचारों को अपनी समालोचना की मुख्य विषय-वस्तु बनाया होता। निःसंदेह, यदि इन विचारों का मूल्यांकन नहीं किया जाता तो यह समझ पाना असंभव है कि किस प्रकार पुरातन ऋषिगण मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में ही ऐसे निष्कर्षों तक पहुँच गए जो कि, चाहे स्वीकार किए गए हों या संशय किए गए हों, आत्म-विश्वासी आधुनिक बुद्धि के भी आश्चर्य एवं प्रशंसा को जागृत करते हैं...
बौद्धिक खोज की सभी प्रणालियाँ पुष्टिकरण और प्रमाणीकरण के ऐसे किन्हीं साधनों पर आश्रित होने की आवश्यकता अनुभव करती हैं जो उनके निष्कर्षों को अधिकतम सुनिश्चित बनाए रखने हेतु सुरक्षा प्रदान करें तथा मानसिक संशय की सतत् पूछताछ या अन्वेषणशीलता से हमें मुक्त कर एक पूर्ण रूप से सुरक्षित आधार की इसकी माँग को पूरा करें, भले कितने ही अपूर्ण रूप से क्यों न हो। इस प्रकार प्रत्येक की द्विविध गतियाँ होती हैं, एक होती है तीव्र, सीधी, फलदायी किन्तु असुरक्षित जबकि दूसरी होती है अधिक सुविचारित और सुनिश्चित। तत्त्वज्ञान की सीधी प्रक्रिया है अनुमान और उसकी पुष्टिकरण की प्रक्रिया है शाब्दिक तर्क के कठोर नियमों के अंतर्गत विचार अथवा तर्क-वितर्क करना; विज्ञान की सीधी प्रक्रिया है प्रकल्पना या स्थापना (Hypothesis), इसकी पुष्टिकरण की प्रक्रिया है भौतिक परीक्षण द्वारा या फिर किसी प्रकार के इंद्रियगम्य साक्ष्य द्वारा या किसी प्रदर्शन द्वारा सिद्ध करना; इसी प्रकार वेद की प्रणाली की भी द्विविध गतियाँ बताई जा सकती हैं; इसकी प्रकटनकारी प्रणालियाँ सीधी प्रक्रियाएँ हैं और मन तथा शरीर द्वारा अनुभूति पुष्टिकारी प्रक्रिया है। वेद की इन दोनों प्रणालियों में परस्पर संबंध निःसंदेह ही ठीक-ठीक वैसा ही नहीं हो सकता जैसा कि तत्त्वज्ञान तथा विज्ञान की बौद्धिक पद्धतियों में होता है; क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद की प्रकटनकारी प्रणालियाँ अपने आप में ही आत्म-प्रकाशकारी तथा आत्म-औचित्य सिद्ध करने वाली हैं। अंतःप्रकाश का स्वभावमात्र ही होता है एक ऐसी अति-बौद्धिक क्रिया जो हमारी खोज और प्राप्ति से स्वतंत्र उस स्वयं-सत् तथा आत्म-अवलोकनकारी सत्य के स्तर पर होती है....."* इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार हमारे वैदिक ऋषियों ने किन्हीं बौद्धिक तरीकों से नहीं बल्कि अंतर्बोधात्मक क्षमताओं के द्वारा उन गहन सत्यों को प्राप्त किया। परंतु हमारा जिस प्रकार का मानसिक गठन है, उसमें अधिकांशतः हमारा अंतर्बोधात्मक क्षमताओं से लगभग कोई संपर्क नहीं रहता और इस कारण जब वे सत्य किसी मानसिक भाषा में प्रकट किये जाते हैं, जैसा कि गीता करती है, तब हम उन्हें केवल कोई मानसिक सत्य समझने की त्रुटि करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि हमें यह संदेह भी नहीं होता कि हम उन्हें गलत रूप से समझ रहे हैं। इसीलिये श्रीअरविन्द हमें यह चेतावनी देते हैं कि 'हमें बराबर सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा'।
प्रथम छः अध्यायों में ऐसे स्पष्ट लक्षण नहीं दिये गये हैं जो अंतर्निहित सत्य की कुंजी प्रदान करते हों; जहाँ जो कठिनाइयाँ प्रस्तुत हुईं उन्हें लेकर उनका (चलते-चलते) समाधान कर दिया गया है; विवेचन का क्रम कुछ कठिन है और कितनी ही उलझनों और पुनरावृत्तियों में से होकर चलता रहा है; ऐसा बहुत कुछ है जो कथन में समाया तो है पर जिसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाया है।... [उदाहरण के लिए प्रथम छः अध्याय योग में ईश्वर के भाव का समावेश करते हैं, ईश्वर का कर्मों और यज्ञों के भोक्ता प्रभु के रूप में निरूपण है, और इसका संकेत-मात्र किया गया है परंतु अभी तक यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि ये ईश्वर अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं और इन्हीं में वैश्विक अस्तित्व के रहस्य की कुंजी है। इसलिए अक्षर पुरुष से होकर इनकी ओर ऊपर बढ़ने से हमारा अपने कर्मों से आध्यात्मिक मुक्ति पाना और फिर भी प्रकृति के कर्मों में लगे रहना संभव है। परंतु अभी यह नहीं बताया गया कि ये परम् पुरुष, जो यहाँ दिव्य गुरु और कर्म-रथ के सारथी-रूप में अवतरित हैं, कौन हैं अथवा अक्षर पुरुष तथा प्रकृतिस्थ व्यक्तिगत सत्ता से उनके संबंध क्या हैं। न ही यह स्पष्ट है कि उनसे आने वाला कर्मों का संकल्प त्रिगुणमय प्रकृति की इच्छा से किस प्रकार भिन्न हो सकता है। यदि वह वही इच्छा हो तो इसका अनुसरण करने वाला जीव, अपने आत्म-भाव में न सही, पर अपने कर्म में तो त्रिगुण के बंधन से कदाचित् ही बच सकता है; और, यदि यही बात है तो जिसका वादा किया गया है वह मुक्ति या तो भ्रांतिपूर्ण बन जाती है या फिर अधूरी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संकल्प सत्ता के कार्यकारी अंश का एक पहलू है, प्रकृति की शक्ति और सक्रिय ऊर्जा, - 'शक्ति, प्रकृति' है। तो क्या त्रिगुणात्मिका प्रकृति से भी उच्चतर कोई प्रकृति है? क्या अहंकार, कामना, मन, इन्द्रिय-समूह, तर्क-बुद्धि और प्राणावेग से भिन्न भी कोई सृष्टि-शक्ति, संकल्प-शक्ति एवं कर्म-शक्ति है?
इसलिए ऐसी संदिग्ध अवस्था में अब जो कुछ करना है वह यही है कि उस ज्ञान को, जिस पर भागवत् कर्मों को आधारित किया जायेगा, और अधिक पूर्णता के साथ बतला दिया जाए। और, वह ज्ञान उन भगवान् के स्वरूप का हो पूर्ण और समग्र ज्ञान हो सकता है जो भगवान् संपूर्ण कर्म के मूलस्रोत हैं और जिनकी सत्ता के अन्दर कर्मयोगी ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब वह उस मुक्त आत्मा को जान लेता है जिसमें से यह अखिल कर्म-प्रवाह निकलता है और उसके मुक्त स्वरूप में भागीदार बन जाता है। इसके अतिरिक्त, उस ज्ञान से वह प्रकाश मिलेगा जिससे गीता के प्रथम भाग के उपसंहार में जो बात कही गयी है उसकी यथार्थता सिद्ध होगी।
-------------------------------
* CWSA 17, p. 551-53
उसे आध्यात्मिक चेतना और कर्म के अन्य सभी हेतुओं और शक्तियों के ऊपर भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करनी होगी; वह ज्ञान समस्त प्राणियों के उन परमेश्वर का ज्ञान होगा केवल जिनके प्रति ही जीव उस पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ अपने-आप को उत्सर्ग कर सकता है जो समस्त प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा है। सातवें अध्याय के प्रारंभ के श्लोकों में भगवान् यही विषय प्रस्तावित करते हैं जो कि उस प्रतिपादन का सूत्रपात करता है जो शेष पुस्तक में प्रतिपादित है।
श्रीभगवान् उवाच
काही में जिन मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ।। १।।
१. श्रीभगवान् ने कहा : हे पार्थ! मुझ में अपने मन को लगाकर, मुझे अपना आश्रय (अपने चित्त और अपने कर्मों का संपूर्ण आधार, निवास-स्थान, आश्रय) बनाकर योगाभ्यास करते हुए पूर्ण रूप में मुझे जिस प्रकार संशय से रहित होकर जानेगा उसे सुन।
क्योंकि वास्तव में तो भगवान् का अपने आप में क्या स्वरूप है इस विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। निरूपण तो केवल उतना ही हो सकता है जितना कि योगाभ्यास करते हुए व्यक्ति को प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य उसे जितना जान सकता है उतना ही निरूपण गीता या अन्य कोई भी सद्ग्रंथ कर सकता है।
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ।। २।।
२. मैं तुझे व्यापक और सविस्तार ज्ञान के साथ उस मूलभूत ज्ञान को कुछ भी छोड़े बिना पूर्ण रूप से कहूँगा, जिसे जान लेने पर इस लोक में फिर और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता।
vii. 19
इस उक्ति का अभिप्राय यह है कि भागवत् सत्ता ही सब कुछ है, वासुदेवः सर्वम्, और इसलिए यदि उन्हें उनकी सब शक्तियों और तत्त्वों के साथ समग्र रूप से जान लिया जाए तो सब कुछ जान लिया जाता है, केवल विशुद्ध आत्मा ही नहीं, अपितु जगत्, कर्म और प्रकृति भी। तब यहाँ जानने की और कोई चीज नहीं रह जाती, क्योंकि वह भगवान् ही सब कुछ है। क्योंकि हमारी दृष्टि यहाँ इस तरह समग्र नहीं है, क्योंकि यह विभाजक मन तथा तर्कबुद्धि पर और विभक्त करने वाले अहंकार के भाव पर आश्रित है, इसलिए वस्तुओं का हमारा मानसिक बोध या अनुभव एक अज्ञान है। हमें इस मन-बुद्धि और अहंकारमय दृष्टि से दूर हटकर सच्चे एकीकारी ज्ञान तक पहुंचना होगा, और उस ज्ञान के दो पहलू हैं, एक ज्ञान है मूलभूत अथवा तात्त्विक, जिसे ज्ञान कहते हैं, और दूसरा है व्यापक या सर्वग्राही, जिसे विज्ञान कहते हैं अर्थात् परम् पुरुष का सीधा आध्यात्मिक अनुभव या बोध है और उसकी सत्ता के विभिन्न तत्त्वों - प्रकृति, पुरुष तथा अन्य सभी - का समुचित अंतरंग ज्ञान, जिसके द्वारा जो कुछ भी है वह अपने भागवत् मूलस्वरूप में तथा अपनी प्रकृति के परम् सत्य में जाना जा सकता है। गीता कहती है कि वह समग्र ज्ञान बड़ी दुर्लभ और कठिन वस्तु है...
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्विद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्विन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।। ३।।
३. सहस्रों मनुष्यों में कोई एकाध ही सिद्धि के लिये प्रयत्न करता है, और जो प्रयत्न करते हैं और सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं उनमें भी कोई विरला ही मुझे मेरी सत्ता के सब सिद्धांतों में, तत्त्व रूप से, जानता है।
इसलिए, उपक्रम के तौर पर तथा इस समग्र ज्ञान को सुप्रतिष्ठित करने के लिए गीता वह गंभीर और महत्त्वपूर्ण भेद प्रस्तुत करती है जो कि इसके संपूर्ण योग का व्यावहारिक आधार है, यह है दो प्रकृतियों का भेद, प्राकृत (phenomenal) और आध्यात्मिक।
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।। ४।।
४. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, (पंच-तत्त्व), मन, बुद्धि और अहंकार - यह मेरी अष्टविध विभक्त प्रकृति है।
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ।। ५।।
५. यह अपरा (निम्नतर) प्रकृति है। हे महाबाहो ! यह भी जान कि इससे भिन्न मेरी अन्य प्रकृति भी है, परा प्रकृति, जो जीव बनती है और जिसके द्वारा यह जगत् धारण किया जाता है।
इसमें सबसे पहले समझने की बात यह है कि आखिर प्रकृति क्या है? जो कुछ भी हम देख, समझ और सुन सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जो भी गहरे या सतही अनुभव हम करते हैं वे सभी प्रकृति के ही कार्यक्षेत्र की चीजें हैं। वहीं, ईश्वर एक ऐसी परम सत्ता हैं जिनका हम अपनी अंतरतम गहराइयों में एक प्रतिबिंब मात्र ही प्राप्त कर सकते हैं। और स्वयं वह प्रतिबिंब भी लगभग प्रकृति का ही बना होता है। वह परम सत्ता तो एक ऐसा तत्त्व है जिसे किसी भी तरीके से, किसी भी अनुभव से या किसी भी सूत्र में हम पकड़ ही नहीं सकते। क्योंकि जिस भी प्रकार से उस तत्त्व का अनुभव करें, उसमें अधिकांशतः तो प्रकृति का ही तत्त्व रहेगा जबकि वह परम सत्ता तो किसी भी अनुभव से पूर्णतः परे है। हम जिसे पुरुष कहते हैं वह भी प्रकृति के अंदर उसी परम सत्ता का ही प्रतिबिंब है। अपने आप में वह परम सत्ता तो सच्चे रूप में चरम-परम है और हमारे किन्हीं भी ऊँचे से ऊँचे सूत्रों या निरूपणों से सर्वथा परे है। इसलिए परम सत्ता के विषय में हमारा यदि कोई अनुभव भी है तो वह मात्र उस प्रतिबिंब का ही अनुभव है और वह भी प्रकृति के दायरे में ही है। सभी उच्चतम संभव लोक भी प्रकृति के ही खेल हैं क्योंकि परम सत्ता तो इन सभी को सूक्ष्म रूप से धारण करते हुए भी, इन सभी में अंतर्निहित होते हुए भी इन सभी से बच निकलती है। अब हालाँकि सभी कुछ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है और कहीं भी किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है तो भी चीजों को समझने की सुविधा के लिए दो प्रकार की प्रकृतियाँ बताई गई हैं। एक है निम्न प्रकृति जो कि अभिव्यक्ति के अंदर हमें इंद्रियों आदि के माध्यम से गोचर होती है, और दूसरी है आध्यात्मिक प्रकृति जो ऊँची से ऊँची आंतरिक चीजों के साथ, वस्तुओं में अंतर्निहित सत्य के साथ व्यवहार करती है। परंतु ये दोनों ही हैं प्रकृति ही और परम तत्त्व इन दोनों से ही छूट निकलता है।
यहाँ गीता का वह प्रथम नवीन तात्त्विक विचार या भाव आया है जो इसे सांख्य-दर्शन के मन्तव्यों से आरंभ करके उनसे भी परे चले जाने में सहायता करता है, और गीता सांख्य की शब्दावली रखते हुए उस शब्दावली को व्यापक अर्थ देते हुए उसे वेदान्तिक अर्थ दे देती है। अष्टधा प्रकृति जो पाँच महाभूतों.... अपनी विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों सहित मन, बुद्धि और अहंकार, यही प्रकृति का सांख्य के अनुसार वर्णन है। सांख्य यहीं रुक जाता है, और चूँकि यह यहीं रुक जाता है, इसे पुरुष और प्रकृति के बीच एक ऐसा भेद करना होता है जिसे मिलाया न जा सके; इस कारण उसे इन दोनों को सर्वथा भिन्न मूल सत्ताओं के रूप में अवस्थित करना पड़ता है।
-----------------------------
* सब लोकों के ऊपर स्थित वह उनको संभाले हुए है,
एकमात्र सर्वशक्तिशालिनी वह 'देवी' नित्य-प्रच्छन्न,
जिसका कि यह जगत् रहस्यमय मुखौटा है;
युग-युगान्तर जिसकी गति के पदक्षेप हैं,
उनकी घटनाएँ उसके विचारों की एक रूपाकृति है,
और सकल सृष्टि उसकी अंतहीन कृति है।
गीता को भी, यदि वह यहीं रुक जाती तो, परम् पुरुष और विश्व-प्रकृति के बीच यही असाध्य विच्छेद स्थापित करना पड़ता और तब यह विश्व-प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया मात्र और यह सारा वैश्विक अस्तित्व महज उस माया का ही परिणाम रह जाता; इसके अतिरिक्त (प्रकृति और इसके इस विश्व-प्रपंच का) और कोई भी अर्थ न होता। परंतु इसके अतिरिक्त भी कुछ है, एक उच्चतर तत्त्वत, एक आत्मा की प्रकृति भी है, पराप्रकृतिर्मे। भगवान् की एक पराप्रकृति है जो इस विश्व के अस्तित्व का मूल कारण है, इसकी मूलभूत सृष्टि-शक्ति और कर्म-शक्ति है; जिसकी कि यह दूसरी, निम्नतर और अज्ञानमयी प्रकृति, केवल एक उपज तथा एक अंधकारमय छायामात्र है। इस पराशक्ति के अन्दर पुरुष और प्रकृति एक हैं। प्रकृति वहाँ पुरुष की संकल्प-शक्ति और कर्ती-शक्ति है, उसकी सत्ता या अभिव्यक्ति की क्रिया है, - कोई पृथक् वस्तु नहीं, वरन् पुरुष स्वयं ही शक्तियुक्त है।
यह हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार मूल प्रकृति से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियाँ, इंद्रियों से तन्मात्राएँ और उनसे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। यही इन चौबीस तत्वों के द्वारा सांख्यों का प्रकृति का विश्लेषण है। इसमें निम्न अष्टधा प्रकृति अहंकार, बुद्धि, मन और इंद्रियों से बनती है। मनुष्य का सारा क्रियाकलाप इस निम्न प्रकृति के अंतर्गत ही रहता है। इसमें भी अधिकांशतः मनुष्य अपनी बुद्धि में तो रहता ही नहीं है। वह तो लगभग अपने मन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों, संवेदनों आदि में ही रमण करता रहता है। शुद्ध रूप से बुद्धि के क्षेत्र तक तो कोई-कोई ही पहुँचता है। इसलिये जब इस प्रकार की हमारी प्रकृति है तब परम प्रभु का, आत्म-तत्त्व का तो इससे कोई तालमेल ही नहीं बैठता। इस निम्न प्रकृति में ऊँचे से ऊँचा तत्त्व बुद्धि है और वह बुद्धि भी सात्त्विकता के बंधन से ऊपर नहीं जाती। इसके स्पष्टीकरण के तौर पर अद्वैत आदि विचारधाराएँ कहती हैं कि आत्म-तत्त्व ही वास्तविक तत्त्व है जबकि यह निम्न प्रकृति तो मानो उसके ऊपर पड़ा एक आवरण है। इसलिए इस आवरण के कारण से ही हमें यह जगत् इस प्रकार का गोचर होता है जबकि वास्तव में यह सब एक प्रकार का भ्रम है, माया है। वास्तविक सत्य तो अध्यात्म तत्त्व है। उसी में एकत्व भाव है। निम्न प्रकृति के सारे विभाजन वहाँ मिट जाते हैं। इसलिए उनके अनुसार मनुष्य का सच्चा कार्य है इस सब प्रपंच से दूर हटकर उसी तत्त्व की ओर जाना। गीता भी आरंभ में अक्षर ब्रह्म की ओर जाने का उपदेश करती है जो कि सदा शांत, अविनाशी, निर्विकार है। इसी आदर्श को भारतीय परंपरा में दीर्घकाल से पोषित किया जाता रहा है। हालाँकि वैदिक परंपरा ऐसे किसी भी एकांगी दृष्टिकोण का कभी समर्थन नहीं करती, न उपनिषद् ही ऐसे दृष्टिकोण को समर्थन देते हैं। परंतु फिर भी ऐसे विचार परंपरा से प्रचलन में रहे हैं। उसी में पले-बढ़े होने के कारण गीता को उसी धरातल से लेकर अर्जुन को आगे ले जाना होगा। इसीलिये गीता जब अर्जुन को ज्ञान का निरूपण करती है तब वह पूछता है कि जब ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है तब उसे उस घोर कर्म में नियोजित क्यों किया जा रहा है। इसलिए इन सभी प्रश्नों का अभी गीता को उत्तर देना बाकी है। यदि गीता यहीं रुक जाती है तब तो एक अपूरणीय खाई रह जाएगी क्योंकि तब कर्म तो केवल हमारी बुद्धि, मन, प्राण और शरीर के द्वारा ही होगा और इस कारण वह अज्ञानमय ही रहेगा और जो ऐसे कर्म में रत है वह मूढ़ है। परंतु गीता इससे आगे जाती है और कहती है कि इससे भिन्न भगवान् की पराप्रकृति भी है। इसी अध्याय के पाँचवे श्लोक में गीता कहती है 'जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्' अर्थात् 'हे महाबाहो! मेरी पराप्रकृति जीव बनती है जिसके द्वारा यह जगत् धारण किया जाता है।'
पर अब इन दोनों प्रकृतियों को जोड़ने वाली कड़ी कहाँ है। यदि यह संयोजक कड़ी न हो तब तो उस पराप्रकृति का जो भी कोई स्वरूप क्यों न हो, उससे हमारा कोई सरोकार ही नहीं हो सकता। इसलिए इनके बीच एक संयोजक कड़ी है और वह है हमारी अंतरात्मा। अभिव्यक्ति से परे उसे जीवात्मा कहते हैं और अभिव्यक्ति में वह हमारी अंतरात्मा बन जाती है और यही वह संयोजक कड़ी है जो परा और अपरा प्रकृति को जोड़ती है। इसलिए जितने भी बहुपुरुष हैं वे सब भी पराप्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं, उसी के अंश हैं। अपरा प्रकृति में तो पुरुष प्रकृति से भिन्न हैं परंतु पराप्रकृति के अंश हैं क्योंकि पराप्रकृति तो परमोच्च ईश्वर की महाशक्ति ही है और उनसे अविभाज्य रूप से एक है। वह ईश्वर की क्रियाशक्ति है और स्वयं वे ही उसे धारण करने वाले हैं। हालाँकि अपने सच्चे स्वरूप में ईश्वर और उनकी शक्ति अभिन्न हैं, तो भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए यह विभाजन हुआ है। परम तत्त्व ने ही अपने आप को दो तत्त्वों में विभक्त कर लिया ताकि यह सारी सृष्टि-क्रिया संपन्न हो सके। इसका विशद वर्णन श्रीअरविन्द अपने सावित्री महाकाव्य में भी करते हैं कि किस प्रकार ये दोनों एक होते हुए भी अपने आप को दो रूपों में विभक्त कर समस्त क्रीड़ा कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें अनेकानेक स्तरों पर ऐसी विराट् सृष्टि गोचर होती है। इसीलिए जितने भी पुरुष हैं, भले वह अतिमानसिक पुरुष ही क्यों न हो, सभी पराप्रकृति के ही अंश हैं। परंतु साथ ही इसमें एक गूढ़ रहस्य यह है कि हमारे हृदय में विराजमान जो ईश्वर है वह उसका अंश नहीं है। वह तो परात्पर ईश्वर का ही अंश है, उन्हीं की उपस्थिति है, हालाँकि इसकी यहाँ चर्चा करना विषयांतर होगा। पर समझने की बात यह है कि हमारी अंतरात्मा ही वह संयोजक कड़ी है और उसी की सहायता से हम अपनी निम्न प्रकृति के ऊपर क्रिया कर सकते हैं, उसे परिवर्तित और रूपांतरित कर सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए जब व्यक्ति अपनी आत्मा में, अपनी अध्यात्म सत्ता में निवास करना शुरू कर देता है तब उसके यज्ञ का आरोहण होने लगता है। और धीरे-धीरे व्यक्ति इस निम्न प्रकृति की बजाय उच्चतर प्रकृति के द्वारा क्रिया करने लगता है जो कि गुणों से परे है। तब फिर क्रिया के उत्प्रेरण का जो सामान्य क्रम है - कि पहले इंद्रिय-संवेदनों आदि के द्वारा मनस् को सूचना प्राप्त होती है और वह उसे बुद्धि तक भेजता है और वहाँ से निर्णय होता है - उसके अनुसार व्यक्ति कर्म नहीं करता। तब उसे सीधे ही अंतःस्फूर्णा होने लगती है। हालाँकि इससे पूर्व भी सभी कुछ होता तो एकमात्र भगवान् की दिव्य प्रकृति के द्वारा ही है और वही हमारे अवचेतन आदि भागों में आवश्यक भाव, अभीप्साएँ, लालसाएँ, इच्छाएँ-कामनाएँ आदि जैसी आवश्यक होती हैं वैसी जगा कर अपने संकल्प को चरितार्थ करती हैं- और इसी अर्थ में कहा जाता है कि छोटी से छोटी चीज भी भगवान् की इच्छा के बिना नहीं होती – परंतु जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में निवास करता है तब निम्न प्रक्रियाओं को काम में लेने की आवश्यकता नहीं रहती और उसकी क्रिया सीधे ही होने लगती है और भगवान् का संकल्प सीधे तौर पर अपने आप को चरितार्थ करने लगता है। ऐसे लोगों की क्रिया भले ही बाहरी रूप से दूसरे सामान्य लोगों की क्रिया जैसी ही प्रतीत होती हो, परंतु वास्तव में वह क्रिया दिव्य क्रिया होती है। इसीलिए भले ही किसी महापुरुष की दैनंदिन क्रियाएँ सामान्य प्रकार की प्रतीत होती हों तो भी यदि कोई थोड़ा बहुत भी संवेदनशील है उसे उनकी क्रिया में, उनके प्रभामंडल में, उनके वातावरण में एक मूलभूत अंतर महसूस होगा। यही गीता के कर्मों का रहस्य है। यही हमें वह सुदृढ़ आधार प्रदान करता है जिस पर स्थित होकर हम पार्थिव जगत् में गुणों से परे रहते हुए भी क्रिया कर सकते हैं और अज्ञान और माया में फँसने से बच सकते हैं। यदि ऐसा न होता तो पृथ्वी पर मनुष्य के लिए दिव्य जीवन में आरोहण की तो कोई संभावना ही नहीं थी और उसकी परिकल्पना करना सर्वथा विसंगत बात होती। और ऐसे में सामान्यतः इसके उपाय के रूप में जीवन से बच निकलने की जो युक्ति बतायी जाती है वही एकमात्र करने योग्य काम रह जाता। परंतु वह तो इस धरती पर इस सारी मानसिक अभिव्यक्ति को, इस सारी सृष्टि को ही निरर्थक सिद्ध कर देता। परंतु गीता इसका समाधान उस संयोजक कड़ी को प्रदान करके करती है जो निम्न प्रकृति को पराप्रकृति से जोड़ती है। वास्तव में तो निम्न प्रकृति केवल एक प्रतीति मात्र है। यदि पराप्रकृति जीव बनकर जगत् को धारण न करती तब तो निम्न प्रकृति का कोई आधार ही नहीं बचता क्योंकि अपने आप में निम्न प्रकृति में कोई सामर्थ्य नहीं कि जगत् को धारण कर सके और इसे बनाए रख सके। अतः वास्तव में तो सारी क्रिया पराप्रकृति की ही है, परंतु कहीं उसकी क्रिया किन्हीं माध्यमों के द्वारा परोक्ष रूप से होती प्रतीत होती है, तो कहीं सीधे तौर पर। हालाँकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी न किसी अंश में पराप्रकृति की सीधी क्रिया न होती हो। भेद केवल इतना है कि यदि यह क्रिया प्रधानतः माध्यमों के द्वारा होती है तब हम इसे निम्न प्रकृति कहते हैं अन्यथा तो क्रिया परा प्रकृति की ही होती है। और एक चरम दृष्टिकोण से तो यह निम्न और परा का भेद भी जब तक दिव्य प्रकृति को भाता है तब तक ही चलता है अन्यथा नहीं। त्रिगुण आदि भी हमें केवल अपने वर्तमान अहमात्मक गठन के कारण ही प्रतीत होते हैं जबकि वास्तव में तो सभी कुछ दिव्य प्रकृति की ही क्रिया है।
आगे इस संयोजक कड़ी का अधिकाधिक निरूपण होगा क्योंकि बिना इसके तो सच्चे कर्म का वास्तव में कोई आधार ही नहीं हो सकता। इन्हीं विषयों को गीता अब विकसित करेगी।
परा-प्रकृति* का अभिप्राय परमात्मा की मूल सनातन प्रकृति और उनकी परात्पर मूल कारण-शक्ति से ही है।
------------------------
* यह पराप्रकृति केवल विश्व के कर्मों में अंतःस्थित भागवत् पुरुष की शक्ति की उपस्थिति मात्र ही नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तब तो केवल वह उस सर्वव्यापक आत्मा की ही निष्क्रिय उपस्थिति होती जो सब पदार्थों में निहित है या जो सब पदार्थों को अपने अन्दर धारण किये है, जो कि एक प्रकार से विश्वकर्म का नियंता तो है पर जो स्वयं सक्रिय कर्ता नहीं है। और न ही यह पराप्रकृति सांख्यों का वह 'अव्यक्त' ही है जो व्यक्त सक्रिय अष्टविध प्रकृति की आदि अव्यक्त बीज-स्थिति है जिसे उत्पादक मूल प्रकृति कहते हैं और जिसमें से उसकी अनेक उपकरणीय और कार्यकारी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। और, 'अव्यक्त' के भाव की वेदान्तिक अर्थ में व्याख्या करना और यह कहना भी पर्याप्त न होगा कि यह पराप्रकृति अव्यक्त ब्रह्म या आत्मा में अंतर्ग्रस्त तथा अंतर्निहित शक्ति है जिसमें से विश्व उत्पन्न होता है और जिसमें इसका लय होता है। पराप्रकृति यह तो है ही, पर इससे भी अधिक बहुत कुछ है; उपर्युक्त तो उसकी अनेकों आत्मस्थितियों में से केवल एक है।
... पराप्रकृति परम् पुरुष की पूर्ण चित्-शक्ति है जो जीव और जगत् के पीछे है। अक्षर पुरुष के अन्दर यह आत्मा में अंतर्निहित रहती है; वह वहाँ होती अवश्य है, पर निवृत्ति में, अपने को कर्म से हटाए हुएः यही क्षर पुरुष और विश्व में बाहर आकर कर्म में प्रवृत्त होती है, प्रवृत्ति में आ जाती है। वहाँ अपनी सक्रिय शक्तिशाली उपस्थिति द्वारा आत्मा में सर्वभूतों को उत्पन्न करती है और उन भूतों में उनकी उस मूल आध्यात्मिक प्रकृति, अर्थात् उनके आंतरिक और बाह्य विषयों की क्रीड़ा के पीछे के चिरंतन सत्य, के रूप में प्रकट होती है। यही वह मूलभूत गुण या भाव और शक्ति अर्थात् 'स्वभाव' है जो सबके होने का, प्राकृत रूप में आने का आत्म-तत्त्व है, उनके लौकिक अस्तित्व के पीछे अंतर्निहित तत्त्व व भागवत् शक्ति है। त्रिगुण की साम्यावस्था इस पराप्रकृति-तत्त्व से उत्पन्न होनेवाली एक परिमेय (quantitative) एवं सर्वथा गौण क्रीड़ामात्र है। अपरा प्रकृति का यह सारा नामरूपात्मक कर्म, यह समस्त मनोमय, इन्द्रियगत और बौद्धिक व्यापार केवल एक बाह्य प्राकृत दृश्य है जो उसी आध्यात्मिक शक्ति और 'स्वभाव' के कारण ही संभव होता है, एकमात्र उसी से इसकी उत्पत्ति है और उसी में इसका निवास है, उसी से यह है।.... परम् आत्मा में से इसी चित्-शक्ति का प्रकट होना ही उत्पत्ति है, परा प्रकृतिर्जीवभूता, क्षर जगत् में उसकी यह प्रवृत्ति है; और परम् आत्मा की अक्षर सत्ता और स्वात्मलीन शक्ति के अन्दर इस चित्-शक्ति का अन्तर्वलयन होने से कर्म की निवृत्ति ही प्रलय है।
चित्-शक्ति के उदय के साथ ही सब उत्पत्ति होती है क्योंकि उसी के अभ्युदय के साथ द्रष्टा भाव आता है अन्यथा तो अवलोकनकारी चेतना ही नहीं होती और उसके अभाव में तो परम तत्त्व का अपने आप में जो भाव होता होगा उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह तो वैसे ही होगा जैसे कि एक कवि के चित्त में कितनी भी गर्भित रचनाएँ क्यों न हों, परंतु यदि वह उन्हें अभिव्यक्त न करे तो दूसरों के लिए तो वे अगम और कल्पना से परे ही होती हैं। वैसे ही बिना चित् शक्ति के परमात्मा के अंतर्निहित तत्त्व तो अभिव्यक्त ही नहीं होते। इसलिए जब चित् शक्ति अपने आप को अभिव्यक्ति से पीछे खींच लेती है तो कर्म की निवृत्ति हो जाती है और उसे हम प्रलय कहते हैं। और यह पीछे खींच लेने की क्रिया भी परा प्रकृति के एक अंश में ही होती है क्योंकि उस प्रलय में भी परा प्रकृति तो फिर भी सदा ही मौजूद रहती है।
इस प्रकार, परा प्रकृति स्वयंभू परम् पुरुष की अनन्त कालातीत सचेतन शक्ति है जिसमें से विश्व के सब भूत आविर्भूत होते हैं और कालातीतता से निकल कर 'काल' में आते हैं। परंतु जगत् में इस अनेकविध वैश्विक संभूति (अभिव्यक्ति) को आत्मा का आधार प्रदान करने के लिए परा प्रकृति अपने आप को जीव के रूप में रूपायित करती है।... जीव ही विविध अस्तित्व का आधार है; यदि हम चाहें तो कह सकते हैं कि यह बहु पुरुष है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि जिस बहुत्व को हम यहाँ अनुभव करते हैं यह उसकी आत्मा है। वह अपने स्वरूप में भगवान् के साथ सदा एकात्म है, भिन्न है केवल अपने स्वरूप की शक्ति में, इस अर्थ में भिन्न नहीं है कि वह वही समान शक्ति नहीं है, अपितु इस अर्थ में कि वह आंशिक अनेकविध वैयक्तिक क्रिया में केवल एक शक्ति को आश्रय प्रदान करता है। इसलिए सभी पदार्थ आदि में, अंत में और अपने स्थितिकाल में तत्त्वतः आत्मा या ब्रह्म ही हैं। सबका मूल स्वभाव आत्मा का स्वभाव ही है, और केवल भेदात्मक निम्न भाव में वे कुछ और दिखाई देते हैं, अर्थात् शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और इन्द्रिय-रूप प्रकृति दिखाई देते हैं। पर ये बाह्य गौण व्युत्पन्न रूप हैं, वे हमारे स्वभाव और हमारे अस्तित्व के मूलभूत सत्य नहीं हैं।
----------------------------
* हमें ध्यान रखना होगा कि हम यह समझने की भूल न कर बैठें कि यह परा प्रकृति काल में अभिव्यक्त जीव ही है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है अथवा यह कि यह केवल संभूति की ही प्रकृति है और आत्मसत्ता की प्रकृति बिल्कुल भी नहीं हैः यह परम् पुरुष की परा प्रकृति का स्वरूप नहीं हो सकता। काल में भी यह परा प्रकृति इससे अधिक कुछ है; अन्यथा जगत् में इसका सत्य केवल अनेकविधता की ही प्रकृति होता और संसार में कोई ऐक्य की प्रकृति न होती। गीता ऐसा नहीं कहतीः वह यह नहीं कहती कि परा प्रकृति अपने सारस्वरूप में स्वयं ही जीव है, जीवात्मिकाम्, अपितु यह कहती है कि वह जीव बन गई है, जीवभूताम्: इस जीवभूता शब्द में ही यह निहित है कि जीव के रूप में अपनी इस बाह्य अभिव्यक्ति के पीछे यह परा प्रकृति अपने मूल रूप में इससे भिन्न और उच्चतर है, यह एकमेवाद्वितीय परम् पुरुष की निज प्रकृति है।
यदि परा प्रकृति केवल जीव ही होती तब तो अनेकविधता में कभी ऐक्य हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके बीच तो कोई एकीकारक शक्ति ही न रहती और ऐसे में तो द्वैतता ही रहती। यही कारण है कि सांख्य में द्वैतता रहती है। सांख्य के अनुसार जब प्रकृति शांत हो जाती है तब जीव मुक्त हो जाता है और इस जगत् प्रपंच के भ्रम से निकल जाता है। परंतु इस दृष्टिकोण में तो ऐक्य का कोई आधार ही नहीं है। परंतु गीता इसे स्वीकार नहीं करती। गीता कहती है कि भले परा प्रकृति ही जीव बनी है परंतु वह केवल जीव ही नहीं अपितु इससे बहुत कुछ और भी है। सारी प्रतीतियाँ भी उस परा प्रकृति के ही रूप हैं। इसीलिए अंततः सभी कुछ एक ही है। संपूर्ण ब्रह्माण्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परा प्रकृति का ही क्षुद्र अंश न हो। और चूँकि सभी उसी के अंश हैं इसलिए सभी एक हैं। जिसे हम माया कहते हैं वह भी उसी परा प्रकृति का ही एक अंधतर रूप है। उसी में से अनेकानेक पुरुष भी उत्पन्न होते रहते हैं।
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।। ६।।
६. इस (परा प्रकृति) को समस्त भूतों का गर्भ-स्थान (अर्थात् जननी) जान; मैं संपूर्ण जगत् की उत्पत्ति हूँ और इसका लय भी हूँ।
यहाँ इस तरह परम् पुरुष, पुरुषोत्तम, और परा प्रकृति को एकीभूत कर दिया गया है; उन्हें एक ही यथार्थता को देखने के दो तरीकों के रूप में रखा गया है। क्योंकि जब श्रीकृष्ण यह घोषित करते हैं कि मैं ही इस जगत् को उत्पत्ति और प्रलय दोनों हूँ, तो यह प्रत्यक्ष है कि उनकी सत्ता की यह परा-प्रकृति ही है जो ये दोनों ही चीजें हैं। अपनी अनन्त चेतना में परम् पुरुष ही आत्मा है और परा-प्रकृति इस आत्मा की सत्ता की अनंत शक्ति या संकल्प है, - यह अपनी अंतर्निहित या सहज दिव्य शक्ति और परम् दिव्य कर्म से संपन्न उनकी अनन्त चेतना ही है...।
इस तरह, परमात्मा या अध्यात्म सत्ता की परा प्रकृति हमें सत्ता का विश्वातीत मूलभूत सत्य और शक्ति, तथा विश्व के अंदर अभिव्यक्ति के लिए आध्यात्मिक सत्य का प्रथम आधार दोनों ही प्रदान करती है। परन्तु उस परा प्रकृति और इस अपरा प्रकृति में संयोजक कड़ी कहाँ है?
परमेश्वर और परा प्रकृति दोनों अविभाज्य रूप से अभिन्न हैं। केवल बौद्धिक निरूपण के लिये यह भेद किया जाता है अन्यथा वास्तव में तो उनमें कोई भेद नहीं है। वैसे ही जैसे कि सच्चिदानंद भी तीन चीजें नहीं है, वह तो एक ही तत्त्व है जिसके तीन लक्षण हैं। ऐसा भी नहीं है कि सच्चिदानंद में तीन चीजें अभिन्न रूप से एक हैं, बल्कि कोई विभाजन है ही नहीं कि एक या अनेक की कोई बात की जाए। उसी प्रकार परमेश्वर और परा प्रकृति में कोई भी विभाजन नहीं हो सकता। हालाँकि पुरुष और प्रकृति के बीच तो कोई विभाजन किया जा सकता है परंतु परा प्रकृति और परमेश्वर में कोई भी भेद नहीं हो सकता। कई बार हम परम तत्त्व और परा प्रकृति की एकता बताने के लिए सूर्य और उसके प्रकाश, अग्नि और उसके तेज की अभिन्नता जैसे कई उदाहरण देते हैं, परंतु परा प्रकृति और परमेश्वर तो तत्त्वतः इतने एकमय हैं कि ऐसे कोई भी उदाहरण उनकी एकता को सही रूप में निरूपित नहीं कर सकते। भेद केवल तब आता है जब यहाँ हम इसका निरूपण करते हैं। जब हम अपने आप में अंतर्निहित हैं, आत्मस्थित हैं, अपनी गहन आंतरिक चेतना में हैं और कोई अभिव्यक्ति नहीं है तब उस भाव को आत्मा, परमात्मा या इसी प्रकार की अन्य कोई संज्ञाएँ देते हैं। और ज्यों ही उस भाव में अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई संकल्प उदित होता है तो उसे हम परा प्रकृति कह देते हैं। और जिसे हम परा प्रकृति कहते हैं वह यदि उस आत्मस्थित भाव में बाहर अभिव्यक्त न हो, या फिर क्रियाशील न हो तो भी भीतर तो वह अस्तित्वमान रहती ही है क्योंकि बाहर अभिव्यक्त होने या न होने से उसके अस्तित्व में अंतर नहीं पड़ता। परम तत्त्व में सभी संभावनाएँ गर्भित हैं, कोई भी नई चीज या तत्त्व नहीं आ सकता। और जब परम तत्त्व स्वात्मलीन होता है तब ऐसे में कोई अभिव्यक्ति नहीं होती और जब उसमें किसी प्रकार का कोई संकल्प उदय होता है तब उसकी क्रियाशक्ति परा प्रकृति अभिव्यक्ति में प्रकट हो जाती है अन्यथा वह उसी परम तत्त्व में अंतर्निहित रहती है। इसलिए परमेश्वर और परा प्रकृति में कहीं कोई भेद ही नहीं है। जब हम चेतना की श्रृंखला में नीचे उतरते हैं केवल तभी अधिकाधिक यह भेद होता पाते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि उस परम तत्त्व के दो भाव हैं। एक भाव है वह जब वह अपने आप में लीन रहता है, स्वात्मकेंद्रित रहता है, तब कोई अभिव्यक्ति आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और दूसरे भाव में वह अभिव्यक्ति की ओर अभिमुख होता है तो इसे परा प्रकृति कहते हैं। असंख्यों ब्रह्माण्ड, अनेकानेक स्तरों पर अनेकानेक जगत् और सृष्टियाँ तथा उनके प्रलय आदि तभी हो सकते हैं जब परम तत्त्व ने अभिव्यक्ति की ओर अपने को अभिमुख किया हो क्योंकि जब वह परम तत्त्व अपने अंतर में ही निहित हो तब तो कोई सृष्टि या प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यह संपूर्ण ब्रह्माण्ड और कुछ नहीं केवल परा प्रकृति का ही रूप है। उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि जिन क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम की हम बात करते हैं वे भी मूलभूत रूप से परा प्रकृति के ही अंग हैं। गीता कहती है 'पराप्रकृतिर्जीवभूता' अर्थात् परा प्रकृति ही जीव या आत्मा बनी है। इसलिए आत्मा और बाहरी प्रकृति दोनों परा प्रकृति ही है। हालाँकि परा प्रकृति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं परंतु चर्चा की सुविधा के लिए हम इसमें परा और अपरा का भेद करते हैं। जब हम चेतना की निम्नतर श्रेणियों में आते हैं तब हमारी चेतना के लिए परा प्रकृति की क्रिया स्पष्टतः गोचर नहीं होती और तब हम इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। परंतु वास्तव में तो परा प्रकृति के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज है ही नहीं। श्रीअरविन्द के योग में भी परा प्रकृति को, दिव्य प्रकृति जगदंबा को परम स्थान प्रदान किया गया है। यहाँ हमें यह सतर्कता बरतनी होगी कि हम जो सामान्य पुरुष-प्रकृति का जैसा भेद करते हैं इसे वैसा न समझ बैठना चाहिये। सांख्यों का जो पुरुष-प्रकृति का भेद है उसमें तो उनके बीच एक भारी खाई है और इसीलिए कर्म का कोई आधार नहीं रहता। परंतु भगवान् की दिव्य प्रकृति में तो क्षर-अक्षर सभी समाहित हैं इसलिए इस भाव में कर्मों को विजयी रूप से किया जा सकता है और ऐसे भाव में त्रिगुणों का तो कोई प्रभाव ही नहीं होता। अवश्य ही बाहरी प्रतीति में हमें वे कर्म त्रिगुणमय प्रतीत हो सकते हैं पर वास्तव में तो वे एक दूसरी ही चेतना से संचालित होते हैं जिस पर गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। अर्जुन भी जब पूछता है कि ऐसे भाव में स्थित व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं तब भगवान् उसे कुछ बाहरी लक्षण बताते अवश्य हैं परंतु वे भी मात्र कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो अर्जुन की बुद्धि के लिए ग्राह्य हों क्योंकि वह इतना विकसित नहीं है कि इससे अधिक लक्षण उसे बताए जा सकें और दूसरे, अपने आप में यह भाव या यह तत्त्व इतना गहरा है कि यह किन्हीं भी लक्षणों में बंध भी नहीं सकता। इसलिए हो सकता है कि उस भाव में स्थित व्यक्ति के इस वर्णन के अनुरूप लक्षण हों और यह भी संभव है कि उसमें ऐसे किन्हीं भी लक्षणों का सर्वथा अभाव हो क्योंकि अपने आप में वह भाव और वह स्थिति तो समस्त लक्षणों से, समस्त वर्णनों से, किन्हीं भी मानसिक निरूपणों से - भले ही वे कितने भी ऊँचे क्यों न हों - सर्वथा परे है।
अब आगे इस पर प्रकाश डाला जाएगा कि हालाँकि परा प्रकृति के अतिरिक्त तो किसी चीज का कोई अस्तित्व है ही नहीं तो भी निरूपण के लिए हम परा और अपरा प्रकृति के बीच में भेद करते हैं। तो फिर वह संयोजक कड़ी कौनसी है जो इन दोनों को जोड़ती है। और इस कड़ी को ढूँढ़ना और उसे समझना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारी चेतना में तो हमें इनमें भेद दिखाई देता है।
प्रश्न : अपरा प्रकृति में हमें जो विकृतियाँ दिखाई देती हैं क्या वे परा प्रकृति के कारण ही हैं?
उत्तर : 'विकृतियाँ' तो हम अपने दृष्टिकोण के कारण कहते हैं जबकि वास्तव में तो कोई विकृति है नहीं। जब सभी कुछ स्वयं परा प्रकृति और उनकी क्रिया और उनके संकल्प की ही अभिव्यक्ति है तब विकृति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए एक दृष्टिकोण से तो सब कुछ सर्वांग रूप से पूर्ण है। परंतु इतना कह सकते हैं कि इस प्रकार की सृष्टि के लिए, इस प्रकार के क्रमविकास के लिए, भगवान् की इस प्रकार की विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए जिन्हें हम विकृतियाँ आदि कहते हैं, वे सब भी आवश्यक थीं। ये सभी चीजें, सभी परिस्थितियाँ क्रमविकास के लिए आवश्यक थीं। परंतु अष्टधा प्रकृति के होने के कारण हमारी विभक्त मानसिक चेतना में यदि हमें ये विकृतियाँ नजर न आएँ तो हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। हमारा उन्हें सुधारकर आगे बढ़ने का प्रयास भी परा प्रकृति की ही योजना का एक अंग है। इसे हम अपने अंदर अंतर्निहित एक ऐसे विधान के रूप में देख सकते हैं जो हमें चेतना के अधिकाधिक उच्चतर सोपानों तक उठा ले जाने को प्रेरित करता है। यदि यह अंतर्निहित विधान न हो तो हमारी मानव चेतना में हम कभी आरोहण करने की अभीप्सा ही न करेंगे और अपने वर्तमान स्तर पर ही संतुष्ट बने रहेंगे। और ऐसा करना तो क्रमविकास के सारे उद्देश्य को ही निष्फल बना देना होगा। यदि अज्ञान या अविद्या न हो तो जिसे हम ज्ञान की संज्ञा देते हैं सदा उसी में फंसे रहेंगे। पर भगवत्तत्त्व तो किसी भी ज्ञान में बँध ही नहीं सकता चाहे वह कितना भी ऊँचा ब्रह्मज्ञान ही क्यों न हो। इन सभी विपर्ययों के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज्यों ही मानसिक चेतना आती है त्यों ही वह चीजों को विभक्त करने लगती है। इसीलिए सभी मानसिक सूत्रों के विपर्यय भी अपने उचित समय और उचित स्थान पर उतने ही सही होते हैं। अतः जहाँ भी क्रमविकास की प्रक्रिया है वहाँ इन विपर्ययों का अस्तित्व है। इसलिए परमात्मा एक-अनेक, अनंत-सीमित, सत्य-असत्य, गुण-निर्गुण, वैयक्तिक-निवैयक्तिक, चेतन-अचेतन आदि के हमारे सभी सूत्रों से सर्वथा परे हैं। वे सच्चे रूप में स्वयं-सत्, स्वतंत्र और स्वयंभू हैं।
मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।। ७।।
७. हे धनञ्जय! मुझ से परे अन्य कुछ परम् नहीं है; जो कुछ भी है वह सब मेरे ऊपर ही सूत्र में पिरोये मणियों के समान गुँथा हुआ है।
परन्तु यह केवल एक ऐसी उपमा है जिसे हम एक सीमा तक ही काम में ले सकते हैं, उसके आगे नहीं; क्योंकि सूत्र के द्वारा इन मणियों को केवल परस्पर संबंध में ही बनाए रखा जाता है, और इन मणियों का उस सूत्र के साथ और कोई ऐक्य या संबंध नहीं होता सिवाय इसके कि इस परस्पर संबंध के लिए वे उस पर आश्रित रहते हैं। इसलिए हम इस उपमा से उस उपमेय की ओर ही चलें जिसकी कि यह उपमा है। परमात्मा की पराप्रकृति अर्थात् परमात्मा की अनन्त चेतन-शक्ति ही, जो आत्मविद्, सर्वविद् और सर्वज्ञ है, इन सब गोचर पदार्थों को परस्पर संबद्ध किये रखती है, उनके अन्दर व्याप्त होती है, उनमें निवास करती तथा उन्हें धारण करती है और उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की व्यवस्था के अन्दर बुन लेती है। यही एक परा शक्ति न केवल सबके अन्दर 'एकमेव' के रूप में प्रकट होती है अपितु प्रत्येक के अन्दर जीव के रूप में, अर्थात् व्यष्टिगत अध्यात्म-उपस्थिति के रूप में भी प्रकट होती है; यही प्रकृति के संपूर्ण त्रैगुण्य के सार-रूप में भी प्रकट होती है। अतएव ये समस्त दृश्य जगत् के पीछे प्रच्छन्न अध्यात्म-शक्तियाँ हैं। यह परम् गुण त्रिगुण की क्रिया नहीं है, त्रिगुणों के कर्म तो गुणों का ही क्रिया-व्यापार है, उनका आध्यात्मिक सार-तत्त्व नहीं। अपितु, वह सार-तत्त्व अंतर्निहित, एकमेव तत्त्व है, जो कि एकमेव होने पर भी इन सभी ऊपरी विविधताओं की भिन्न-भिन्न अंतःशक्ति भी है। यह दिव्य संभूति (Becoming) का मूलभूत सत्य है, एक ऐसा सत्य जो इसकी सभी बाह्य प्रतीतियों को धारण करता है तथा उन्हें आत्मिक तथा दिव्य अर्थ प्रदान करता है।
अतः हमारे अंदर जो आत्मतत्त्व है, वही अपरा को परा प्रकृति से जोड़ता है। परा प्रकृति ही एकमेवाद्वितीयं है। जब व्यक्ति अपने आत्मतत्त्व में स्थित होता है तब वह अपने मानसिक और प्राणिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और इन पर शासन कर सकता है, इन्हें संशोधित और रूपांतरित कर सकता है। त्रिगुणों का सारा आधार हमारी चैत्य सत्ता, हमारी आत्म सत्ता पर ही आधारित है। व्यष्टिगत आत्मा ही इनका आधार है और वही परा प्रकृति की क्रिया के साथ इन्हें जोड़ती है। गीता के अंदर आगे चलकर स्वभाव और स्वधर्म का वर्णन आएगा। एक होती है हमारी बाह्य त्रिगुणमयी प्रकृति और इसके पीछे होता है हमारा 'स्वभाव' अर्थात् वह विशिष्ट आंतरिक गठन जिसके द्वारा हमें अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति करनी होती है। और उस स्वभाव के पीछे होता है मद्भाव। इसलिए यह स्वभाव ही बाह्य प्रकृति और मद्भाव के बीच की कड़ी है। भारतीय संस्कृति में सदा ही यह बात सुविज्ञात रही है इसलिए सदा ही स्वभावनियत कर्म पर बल दिया जाता रहा है। कहने का अर्थ है कि जीव के अंदर जो व्यष्टिगत आत्मतत्त्व है, जो दिव्य संभूति है, भगवान् की वैयक्तिक दिव्य उपस्थिति है वह परा प्रकृति की ही संभूति है और उसी के द्वारा वह अभिव्यक्त होती है और वही वह तत्त्व है जो हमें परा प्रकृति से जोड़ता है।
vii. 12
त्रिगुणों की क्रियाएँ तो बुद्धि, मन, इन्द्रिय, अहंकार, प्राण तथा जड़ पदार्थ के केवल सतही अस्थिर भाव हैं 'सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च', जबकि यह सारभूत तत्त्व 'स्वभाव' अर्थात् संभूति की मूल सनातन अंतःशक्ति है। यही 'स्वभाव' समस्त भूतभाव या अभिव्यक्ति का तथा प्रत्येक जीव का मूल विधान है; यही प्रकृति का मूल तत्त्व है और यही प्रकृति के विकास का कारण है। यह प्रत्येक प्राणी में निहित तत्त्व है, जो कि परात्पर भगवान् के ही आत्माविर्भाव से, ईश्वर के 'मद्भाव' से निकलता है और उससे सीधे सम्बद्ध रहता है। भगवान् के इस 'मद्भाव' का 'स्वभाव' के साथ और 'स्वभाव' का बाह्य भूतभावों के साथ अर्थात् भगवान् की परा प्रकृति का व्यष्टिपुरुष की आत्मप्रकृति के साथ और इस विशुद्ध मूल आत्मप्रकृति का त्रिगुणात्मिका प्रकृति की मिश्रित और द्वन्द्वमय क्रीड़ा के साथ जो सम्बन्ध है उसी में उस परा शक्ति और इस अपरा प्रकृति के बीच की कड़ी मिलती है। अपरा प्रकृति की विकृत शक्तियाँ और उसकी संपदाएँ उसे परा प्रकृति की परम शक्तियों और सम्पदाओं से ही प्राप्त हैं और इसलिए अपरा प्रकृति की शक्तियों और संपदाओं को अपना मूलस्रोत और वास्तविक स्वरूप तथा अपने सब कर्मों और गतियों के मूल धर्म को जानने के लिए परा शक्ति की शक्तियों और संपदाओं के समीप लौट जाना होगा। इसी प्रकार यह जीव, जो यहाँ प्रकृति के गुणों की बंधनयुक्त, दीन और निम्नतर क्रीड़ा में लिप्त है, यदि इससे निकलकर दिव्य और पूर्ण होना चाहे तो, उसे अपने स्वभाव के मूलभूत गुण के विशुद्ध कर्म का आश्रय लेकर अपने स्वयं के स्वरूप के उस उच्चतर धर्म में लौट जाना होगा जिसमें वह अपनी दिव्य भागवत् प्रकृति के संकल्प, शक्ति, सक्रिय तत्त्व और परम् कर्मभाव को खोज सकता है।
जैसा कि पहले भी यह विशद चर्चा हो चुकी है कि स्वभावों को मोटे रूप से चार श्रेणियों में बाँटा गया है और ये चार श्रेणियाँ जगदंबा की चार महाशक्तियों - महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती - पर आधारित हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति के स्वभाव में ये चारों ही महाशक्तियाँ सदा मौजूद रहती हैं, फिर भी इनमें से किसी एक या अधिक का प्रभाव अधिक हो सकता है और उसी के आधार पर उसका स्वभाव तय होता है। परंतु किसी एक स्वभाव के अंतर्गत भी अनंत विविधताएँ होती हैं। उदाहरण के लिए क्षत्रिय स्वभाव होने पर भी कोई भी दो क्षत्रिय एक समान नहीं होते और प्रत्येक में एक विशिष्ट प्रकार का संतुलन होता है और वह भी समय-समय पर भिन्न-भिन्न होता रहता है। इस स्वभाव का पालन करना ही स्वधर्म है। परंतु इस स्वभाव का पालन करना तभी तक आवश्यक माना जाता था जब तक कि व्यक्ति इतना विकसित न हो जाए कि वह सचेतन रूप से किसी दिव्य मार्गदर्शन का अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाए। यह दिव्य मार्गदर्शन किसी गुरु के रूप में, किसी पुस्तक के रूप में या फिर अन्य किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। और जब यह मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तब व्यक्ति पग-पग पर अपने अहं के स्थान पर उसे प्रतिष्ठित करके आगे बढ़ सकता है। तब फिर व्यक्ति को अपने स्वभाव आदि के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि अब उसे सीधे ही गुरु द्वारा दिशानिर्देश प्राप्त होने लगते हैं। उदाहरण के लिए श्रीअरविन्द आश्रम के अंदर श्रीमाताजी की शरण में आने के बाद व्यक्ति को इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि उसका स्वभाव क्षत्रिय का है या ब्राह्मण का या फिर अन्य किसी का। उनकी शरण में आने पर तो फिर वे ही वास्तव में जानती हैं कि व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म कौनसा है और उसी का पालन करना व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्यं कर्म बन जाता है।
यह बात इसके तुरंत बाद वाले श्लोकों से ही स्पष्ट हो जाती है जिसमें गीता यह दर्शाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि किस प्रकार भगवान् अपनी परा प्रकृति की शक्ति से इस विश्व के चेतन तथा अचेतन कहे जानेवाले प्राणियों में अभिव्यक्त होते हैं और उनमें क्रिया करते हैं।
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ।। ८।।
८. हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! मैं जलों में रस' हूँ, चन्द्रमा और सूर्य का प्रकाश हूँ, समस्त वेदों में प्रणव (प्रणवाक्षर ॐ) हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में मनुष्यत्व हूँ।
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्वास्मि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।। ९।।
९. और मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ, सभी भूतों में (उनका) जीवन हूँ, तपस्वियों में मैं तप हूँ।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।। १० ।।
१०. हे पृथापुत्र अर्जुन! मुझे समस्त भूतों का सनातन बीज जान; मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ।
प्रत्येक दृष्टांत में उस मूलभूत गुण की ही ऊर्जा है जिसे उस विशिष्ट लक्षण के रूप में दिया गया है जो उन भूतों की प्रकृति में भागवत् शक्ति का संकेत करता है - उन सब भूतों में से प्रत्येक जो कुछ भी वह इस अभिव्यक्ति में बन गया है उसके लिए वह इस मूलभूत गुण की ऊर्जा पर ही निर्भर करता है। भगवान् फिर कहते हैं, "सभी वेदों में मैं प्रणव हूँ,” अर्थात् वह मूल ध्वनि ॐ हूँ जो श्रुति-प्रकाशित शब्द की समस्त शक्तिशाली सृजनात्मक ध्वनियों का आधार है; ॐ ही ध्वनि और वाणी की शक्ति का वह एकमात्र सार्वभौमिक संविन्यास या सूत्रण है जो कि वाक् और शब्द की समस्त आध्यात्मिक शक्ति और अंतर्निहित संभावना समाहित रखता है और उन्हें एकत्रित रखता है, इन शक्तियों और संभावनाओं को समन्वित करता है और इन्हें अपने अंदर से उन्मुक्त करता है, प्रकट करता है। इसी में से वे अन्य ध्वनियाँ निकलती और इसी का विकास मानी जाती हैं जिनमें से भाषाओं के शब्द निकलते और बुने जाते हैं। इससे यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। इन्द्रियों के, प्राण के, ज्योति, बुद्धि, तेज, बल, पौरुष, तप आदि के बाह्य प्राकृत विकास परा प्रकृति की चीज नहीं हैं। परा प्रकृति अपनी आत्मस्वरूप शक्ति में वह मूलभूत गुण है जो 'स्वभाव' का गठन करती है। आत्मा की जो शक्ति इस प्रकार व्यक्त हुई है, चेतना की ज्योति तथा वस्तुओं में उसके तेज की जो शक्ति है जो अपने विशुद्ध मूल स्वरूप में प्रकट हुई है, वही आत्म-स्वभाव है। वह ऊर्जा, ज्योति, शक्ति ही वह सनातन बीज है जिसमें से अन्य सब चीजें विकसित और उत्पन्न हुई हैं तथा इसी की परिवर्तनशीलताएँ और लचीली अवस्थाएँ हैं। इसीलिए इस श्रृंखला के बीच में गीता एक सर्वसामान्य सिद्धान्त के तौर पर यह बात कह जाती है कि, "हे पार्थ, मुझे सब भूतों का सनातन बीज जान।" यह सनातन बीज आत्मा की शक्ति, आत्मा की सचेतन इच्छा है, वह बीज है जिसे, गीता ने जैसा कि अन्यत्र बतलाया है कि, भगवान् महत् ब्रह्म में, विज्ञान xiv3 विस्तृतता में आधान करते हैं, स्थापित करते हैं और उसी से सब भूतों की बाह्य जगत् में उत्पत्ति होती है। यही आत्मशक्ति का वह बीज है जो अपने आप को सब भूतों में मूलभूत गुण के रूप में प्रकट करता है और उनका स्वभाव बनता है।
इस मूलभूत गुणरूपा शक्ति और अपरा प्रकृति की इन्द्रियगोचर उत्पत्तियों के बीच, अपनी शुद्धावस्था में मूल वस्तु और उस वस्तु के अपर या निम्नतर बाह्य रूपों के बीच जो यथार्थ भेद है, वह इस श्रृंखला के अन्त में बहुत स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है।
यहाँ मुख्य बात यह है कि अंतर्निहित स्वभाव के रूप में परा-प्रकृति ही प्रकट होती है और स्वभाव ही सभी बाहरी क्रियाकलाप का सनातन बीज है। हालाँकि गीता तो इस विषय में प्रवेश नहीं करती परंतु वेदों में इसका विस्तृत वर्णन है कि किस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि 'शब्द' के स्पंदन से बनती है। श्रीअरविन्द से भी हम यह आशा नहीं कर सकते कि गीता पर अपनी टीका में वे इस विषय को विस्तार से समझाएँ क्योंकि ऐसा करना विषयांतर होगा, पर फिर भी इस ओर वे संकेत अवश्य कर रहे हैं। सभी लोकों में ऊपर से लेकर नीचे तक एक अटूट श्रृंखला है। इसीलिए जब गुह्य जगतों में जाकर व्यक्ति कोई विशिष्ट स्पंदन पैदा करता है तब उसका प्रभाव हमारे भौतिक जगत् तक भी आता है।
-------------------------------
* अर्थात्, अपनी परा प्रकृति में स्वयं भगवान् ही इन सब विभिन्न इन्द्रिय-संबंधों के मूल में स्थित शक्ति या तेज हैं जिनके कि प्राचीन सांख्य प्रणाली के अनुसार (पंचमहाभूत) आकाशीय, तैजस, वैद्युतिक तथा वायवीय, जलीय तथा जड़तत्त्व के अन्य मूलभूत रूप भौतिक माध्यम हैं। ये पंचमहाभूत अपरा प्रकृति के परिमाणात्मक (quantitative) या भौतिक तत्त्व हैं और ये ही सब भौतिक रूपों के आधार हैं। पंचतन्मात्राएँ - रस, स्पर्श, गंधादि - अपरा प्रकृति के गुणात्मक (qualitative) तत्त्व 31 hat 9 तन्मात्राएँ सूक्ष्म शक्तियाँ हैं जिनकी क्रिया के द्वारा ही इन्द्रियगत चेतना का जड़तत्त्व के स्थूल रूपों के साथ सम्बन्ध स्थापित होता है, - वे ही बाह्य सृष्टि के समस्त ज्ञान का आधार हैं। भौतिक दृष्टिकोण से जड़तत्त्व ही यथार्थता है और इन्द्रिय विषय उसी की उपज हैं; परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य इससे विपरीत है। जड़तत्त्व और भौतिक माध्यम स्वयं ही (किसी अन्य सत्ता से) व्युत्पन्न शक्तियाँ हैं और मूलतः केवल ऐसे स्थूल तरीके या अवस्थाएँ हैं जिनमें जगत् के भीतर प्रकृति के त्रिगुण की क्रियाएँ जीव की इन्द्रिय-चेतना के समक्ष प्रकट होती हैं। एकमात्र मूल सनातन सत्य है प्रकृति की ऊर्जा अर्थात् सत्ता की शक्ति व गुणवत्ता जो इन्द्रियों के द्वारा जीव के सम्मुख इस प्रकार स्वयं को प्रकट करती है। और इन्द्रियों के अन्दर जो कुछ सार-तत्त्व है, परम् आध्यात्मिक और अत्यंत सूक्ष्म है, वह तत्त्वतः वही वस्तु है जो वह सनातन गुणवत्ता और शक्ति है। परंतु 'प्रकृति' के अन्दर सत्ता की जो ऊर्जा या शक्ति है वह अपनी निज प्रकृति के रूप में स्वयं भगवान् ही हैं; इसलिए प्रत्येक इन्द्रिय अपने विशुद्ध स्वरूप में वही प्रकृति है, प्रत्येक इन्द्रिय सक्रिय सचेतन-शक्ति में स्थित भगवान् ही है।
हमारे वैदिक ऋषियों का इन जगतों में सहज प्रवेश था जिस कारण वे वहाँ के विधान को इस जड़-जगत् तक के विभिन्न लोकों में क्रियाशील कर सकते थे। इसीलिए वैदिक मंत्र इतने शक्तिशाली हैं। वे अपनी बीज ध्वनि से गुह्य शक्तियों की क्रिया को यहाँ सक्रिय कर सकते हैं जिनका प्रभाव अप्रत्याशित होता है। हमारे ऋषियों ने उस सर्वोच्च सत्य को बिना किसी प्रकार के मिश्रण के बीज मंत्रों के रूप में, वाणी, विचार आदि के रूप में धरती पर प्रकट किया जिनके द्वारा धरती पर सामंजस्य और दिव्यतर चेतना स्थापित की जा सकती है। इन उच्चतर शक्तियों के प्रभाव के कारण ही वैदिक काल में, सतयुग में, निम्नतर शक्तियों को उनकी क्रिया करने का अधिक मौका नहीं मिलता था क्योंकि उन पर उच्चतर शक्तियों का अंकुश रहता था। ऐसे में व्यक्ति स्वभाव नियत कर्म सहज रूप से कर सकता था। परंतु चूँकि आत्मतत्त्व को अधिकाधिक निम्नतर जगतों में उतरकर उनके पदार्थों को अपने हाथ में लेकर उन्हें रूपांतरित करना था इसलिए आत्मतत्त्व को मानसिक, प्राणिक और भौतिक चेतना में उतरना पड़ा जिसके कारण कि पूर्व में निम्नतर चीजों पर जैसा अंकुश था वह नहीं रह पाया। हालाँकि इन सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अब भी सभी कुछ का सनातन बीज वही आत्मतत्त्व ही है। इसलिए कुछ भी निष्फल नहीं हुआ है। इस प्रकार यहाँ इस परा और अपरा प्रकृति के बीच की श्रृंखला बता रहे हैं जिनके बीच की कड़ी है हमारा स्वभाव जो कि परा प्रकृति का ही रूप है। परंतु वह केवल स्वभाव से ही सीमित नहीं हो जाती। वह तो स्वभाव के अलावा और सब कुछ भी है।
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् ।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।। ११।।
११. हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन! मैं बलवान् मनुष्यों में काम और राग से रहित बल हूँ। प्राणियों में ऐसी कामना हूँ जो उनके धर्म के विरुद्ध न हो।
पहला कथन कोई कठिनाई नहीं देता। बलवान् पुरुष के अन्दर बलतत्त्व की भागवती प्रकृति होने पर भी वह पुरुष कामना के और आसक्ति के वश में हो जाता है, पाप में गिर जाता है और पुण्य की ओर जाने के लिए संघर्ष करता है। इसका कारण यही है कि वह अपने समस्त जीवनसंबंधी कर्म करते समय नीचे उतरकर त्रिगुण की पकड़ में आ जाता है, अपने कर्म को ऊपर से, अपनी मूल भागवती प्रकृति के द्वारा संचालित नहीं करता। उसके बल का दिव्य स्वरूप इन निम्न जीवनसंबंधी क्रियाओं से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता, प्रत्येक तमाच्छादन और प्रत्येक स्खलन के बाद भी वह तत्त्वतः वैसा का वैसा ही बना रहता है।... पर भगवान् कामना, 'काम', कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इस कामना को हमारा महाशत्रु बताया गया है जिसे मार डालने को कहा गया है। पर वह कामना तो त्रिगुणात्मिका निम्नतर प्रकृति की कामना थी जिसका मूल उत्पत्ति स्थान तो रजोगुण है, रजोगुणसमुद्भवः; और जब हम कामना की बात करते हैं तो प्रायः हमारा अभिप्राय इसी से होता है। पर यह जो दूसरा आध्यात्मिक है, वह एक ऐसा संकल्प है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है।
क्या इस आध्यात्मिक 'काम' का अभिप्राय पुण्यशील कामना, नैतिक स्वरूप की एक सात्त्विक कामना है, क्योंकि, पुण्य अपनी उत्पत्ति और प्रवृत्ति में सदा सात्त्विक होता है? परन्तु तब तो यहाँ एक प्रत्यक्ष विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, - चूँकि इसके ठीक बाद वाली पंक्ति में सभी सात्त्विक भावों को बताया गया है कि वे भगवद्-जात नहीं अपितु केवल निम्नजात विकार हैं। निःसंदेह यदि किसी को भगवान् के किंचित्-मात्र भी सन्निकट पहुँचना हो तो पाप का परित्याग करना होता है; परंतु इसी प्रकार यदि हमें भागवत्-सत्ता में प्रवेश करना हो तो पुण्य को भी पार कर जाना होता है। पहले सात्त्विक प्रकृति प्राप्त करनी होती है, परंतु बाद में उससे भी परे जाना होता है। नैतिक या सदाचारी कर्म केवल शुद्धि के साधन हैं जिससे हम भागवत् प्रकृति की ओर ऊपर उठ सकते हैं, पर वह प्रकृति स्वयं ही द्वन्द्वातीत होती है, - और वास्तव में, यदि ऐसा न होता, तो विशुद्ध भागवत् उपस्थिति या भागवत् शक्ति किसी ऐसे बलवान् मनुष्य में कभी न रह सकती थी जो राजसिक आवेगों (काम क्रोधादि) के अधीन होता है। आध्यात्मिक अर्थ में धर्म नैतिकता या सदाचार नहीं है। गीता अन्यत्र कहती है कि धर्म वह कर्म है जो 'स्वभाव' के द्वारा अर्थात् अपनी प्रकृति के मूलभूत विधान के द्वारा नियत होता है। और यह स्वभाव अपने सारमर्म में आत्मा की ही अंतःस्थित चिन्मय इच्छा और विशिष्ट कर्मशक्ति का ही विशुद्ध गुण है। अतः कामना का अभिप्राय यहाँ हमारे अन्दर रही हुई उस सोद्देश्य भगवदिच्छा से है जो निम्न प्रकृति के आमोद की नहीं अपितु अपनी ही क्रीड़ा और आत्मपूर्णता के आनन्द की खोज करती और स्वतःसिद्ध है; यह अस्तित्व के उस दिव्य आनन्द की कामना है जो 'स्वभाव' के विधान के अनुसार अपनी सज्ञान कर्मशक्ति को प्रकट कर रहा है।
यहाँ जिस कामना की बात हो रही है उस कामना को भगवद्-संकल्प कहते हैं। मनुष्य की कामना में और उस संकल्प में अन्तर है। भगवान् जब अवतार रूप में प्रकट होते हैं तब भी वे कर्म तो करते ही हैं, यहाँ तक कि घोर कर्म भी करते हैं, परंतु किसी कामना के वशीभूत होकर नहीं अपितु अपने संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में करते हैं। यह संपूर्ण संसार कामना के वशीभूत नहीं अपितु भगवद्-संकल्प के आधार पर चल रहा है जिसमें कामना तो उसे आच्छादित करने वाला एक विकार है जिसे हम अपने अहं आदि के कारण कर्मों में जोड़ते हैं। इसलिए कामना के कारण कर्मों में जो दोष आ जाते हैं वे दोष भगवद्-संकल्प की अभिव्यक्ति रूप कर्म में नहीं रहते। कर्मों में जो समस्याएँ पैदा होती हैं वे तो उसके साथ कामना आदि के जुड़ने से पैदा होती हैं। यह अन्तर समझना बहुत आवश्यक है। इस कामना पर अंकुश लगाने के लिए भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न तरीके के उपाय बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो सात्त्विक और धर्म-सम्मत कार्य हों, समाज के द्वारा स्वीकृत हों केवल वे ही कार्य करने चाहिए। कुछ अन्य लोगों का मत है कि इच्छाओं को जितना अधिक दबाया जाता है वे उतनी ही अधिक बढ़ती हैं इसलिए मर्यादित रूप से इच्छाओं-कामनाओं की तुष्टि स्वीकार्य है। इस तरीके की अनेक विचारधाराएँ प्रचलित हैं। परंतु श्रीअरविन्द कहते हैं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है धरती पर भागवत् साम्राज्य की स्थापना करना जो कि केवल भागवत् इच्छा-शक्ति की अभिव्यक्ति से ही संभव है। इसलिए सच्चे कर्म करने के लिए कामना या संकल्प के बीच का यह भेद जान लेना अत्यावश्यक है। भागवत् इच्छा-शक्ति की अभिव्यक्ति ही कर्म का सच्चा आधार है जिसके बिना संसार में कर्म हो ही नहीं सकते। बिना इस आधार के या तो व्यक्ति पूरी तरह कामना के वशीभूत हो कर्म करता है, या फिर कोई मध्यमार्ग अपनाता है या संन्यासमय जीवन बिताता है या फिर कर्मों को बलात् रोकने का प्रयास करके अपने अंदर द्वंद्व पैदा कर लेता है और अपनी ही शक्ति क्षीण कर लेता है। इन सबका विस्तृत वर्णन तीसरे अध्याय में आ चुका है।
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यक्ति केवल कामना से ही कर्मों को करता है? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कामना के कारण नहीं अपितु यंत्रवत् अथवा अभ्यास के कारण होते हैं। कुछ का उत्प्रेरण अवचेतन भागों से होता है। वास्तव में इन सबके पीछे भागवत् संकल्प ही कार्य करता है। परंतु अहं के कारण हम इनमें कामना के विकार को जोड़ देते हैं जिससे कि कर्म के पीछे हमारे मनोभाव में अशुद्धि आ जाती है। जब हम सचेतन रूप से उस संकल्प से जुड़ जाते हैं तब हमारा शुद्धिकरण हो जाता है और हम भगवान् के यंत्र बन जाते हैं। अन्यथा कार्य तो सदा ही भागवत् संकल्प ही करता है परंतु ऐसा वह अप्रत्यक्ष रीति से, हमारी अवचेतना आदि के माध्यम से इच्छाओं, भयों, कामनाओं, लालसाओं को जब-जहाँ-जैसा आवश्यक हो वैसा भाव उत्पन्न करके करता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपनी कामना के कारण अपने निजी सामर्थ्य के बलबूते पर कुछ भी करने को स्वतंत्र है। परंतु यह एक बड़ी ही हीन प्रक्रिया है जिसमें आत्मा की कोई गरिमा नहीं होती। जब व्यक्ति भागवत् संकल्प की प्रेरणा से कार्य कर रहा हो तो इसका अर्थ है कि उसे कर्म का उत्प्रेरण सीधे ऊपर से ही प्राप्त होता है, अवचेतना आदि के माध्यम से नहीं। यदि यह उत्प्रेरण ऊपर से सीधे ही प्राप्त न हो तो भागवत् संकल्प शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। हालाँकि कर्म तो अंततः सभी भागवत् संकल्प से ही साधित होते हैं परंतु हमारे विकृत मनोवैज्ञानिक गठन के कारण उसके साथ ये कामना आदि विकृतियाँ जुड़ जाती हैं। पर जब एक निश्चित शुद्धिकरण हो जाता है तब हम यह संकल्प सीधे ही प्राप्त कर सकते हैं, किन्हीं अप्रत्यक्ष रीतियों की आवश्यकता नहीं रहती। तब फिर हमारी बुद्धि और मन का हस्तक्षेप कम होता जाता है। संकल्प की क्रिया में कोई भी दोष नहीं होता। तभी तो भगवान् अर्जुन को कहते हैं कि 'यदि मेरे कहने से तू सारे संसार को भी नष्ट कर देगा तो भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और यदि तू धर्म और नैतिकता आदि के विचार से युद्ध करेगा तो तू पाप का भागी होगा और फिर उसके अपने परिणाम होंगे।'
कर्म की सच्ची शक्ति संकल्प से ही प्राप्त होती है जो सभी निम्न विकारों से परे है इसलिये भगवान् सभी कर्म करते हुए भी सभी विकारों से रहित हैं। यह कोई नैतिक आदर्शों के अनुसार किया गया कर्म नहीं है क्योंकि नैतिक आदर्शों के अनुसार करने से कर्म अहं और इच्छाओं आदि से मुक्त नहीं हो जाते। नैतिक आदर्श तो और कुछ नहीं बस ऐसे सामूहिक विधान हैं जो कि मनुष्य की अनियंत्रित पाशविकता पर कुछ अंकुश लगाने का और उसकी मन, प्राण और शरीर की भौंडी तुष्टियों को कुछ अच्छे रंग देने का काम करते हैं ताकि उनका भद्दापन दिखने में उतना भद्दा प्रतीत न हो। सच्चे कर्म तो व्यक्ति में स्वभाव रूप से स्थित भगवान् की भागवत् प्रकृति - परा प्रकृति - द्वारा किये जाते हैं और वे ही स्वभाव नियत कर्म होते हैं।
----------------------------
*इसके लिए III.43 पर की गई व्याख्या देखिए।
प्रश्न : यहाँ कह रहे हैं कि यदि किसी को भगवान् के किंचित्-मात्र भी सन्निकट पहुँचना हो तो पाप का परित्याग करना होता है; परंतु इसी प्रकार यदि हमें भागवत्-सत्ता में प्रवेश करना हो तो पुण्य को भी पार कर जाना होता है। इसका क्या अर्थ है?
उत्तर : चूंकि भगवान् किन्हीं भी नियमों से बाध्य नहीं हैं इसलिए किसी भी अवस्था से व्यक्ति अवश्य ही भगवान् के पास पहुँच सकता है। अधम से अधम व्यक्ति भी एकाएक परमात्मा के पास पहुँच सकता है। परंतु गीता जिस सामान्य क्रम की बात करती है वह है तामसिक से राजसिक और उससे सात्त्विक अवस्था की ओर आरोहण । गीता के सत्रहवें तथा अठारहवें अध्याय में विस्तृत वर्णन है कि किस प्रकार भोजन, यज्ञ, दान, तप, श्रद्धा आदि सभी तामसिक, राजसिक और सात्त्विक प्रकार के होते हैं। सामान्य क्रम में व्यक्ति तामसिक और राजसिक अवस्था से सीधे ही परमात्मा की ओर नहीं जा सकता। इसलिए सात्त्विक गुणों का विकास आवश्यक है। और अंत में सात्त्विकता को भी छोड़ कर आगे जाना होगा क्योंकि आखिर सात्त्विक गुण भी केवल शुद्ध मानसिक दृष्टिकोण के बंधन ही हैं इसलिए ये भी व्यक्ति को परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकते। परमात्मा पाप-पुण्य से परे हैं परन्तु उनका आभास निम्न प्रकृति में रहने पर नहीं हो सकता। भगवान् की भक्ति के द्वारा जब चैत्य विकसित होता है तब उसे कोई भी चीज नहीं बाँध सकती।
प्रश्न : भगवान् के निकट पहुँचने और भगवान् में प्रवेश करने में क्या अन्तर है?
उत्तर : तामसिक और राजसिक गुणों की अपेक्षा सात्त्विक गुण भगवान् के अधिक निकट है परन्तु इससे भी व्यक्ति भगवान् में प्रवेश नहीं कर सकता। श्रीरामकृष्ण जी तामसिक, राजसिक और सात्त्विक का उदाहरण देते हुए इनकी तुलना लोहे, चाँदी और सोने की जंजीरों से करते थे। सात्त्विक मनुष्य के लिए भी भगवान् में प्रवेश करना आसान नहीं है। इसीलिये श्रीकृष्णप्रेम कहते थे कि साधना, मुक्ति की इच्छा, ब्रह्मज्ञान आदि तो सात्त्विक बातें हैं और सात्त्विक व्यक्ति इनकी इच्छा करेगा परन्तु मुकुन्द की सेवा ही है जो नित्रैगुण्य है। वह सभी गुणों से परे है। परन्तु सेवा तो अंतरात्मा का भाव है। बिना अंतरात्मा के भाव के तो सदा लेन-देन या लाभ-हानि का ही विचार रहता है। भगवान् की या श्रीमाताजी की या फिर अपने गुरु की सेवा करने में भी व्यक्ति के मन में यह हिसाब-किताब रहता है कि उससे उसे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो जाएँगे या फिर अन्य दूसरे लाभ प्राप्त हो जाएँगे। इसका विश्लेषण करें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारी दृष्टि में अनुभव आदि हमारे इष्ट से अधिक श्रेष्ठ हो गए और जबकि वे इष्ट तो उन उद्देश्यों की पूर्ति कराने वाले साधन मात्र ही रह गए।
प्रायः ही हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में हम सुनते हैं कि भगवान् की या गुरु की कृपा से व्यापार में लाभ हो गया या फिर नौकरी लग गई, या फिर बेटी की शादी हो गई या फिर ऐसी ही अन्य कोई मनोकामना पूर्ण हो गई। चेतना के ऐसे स्तर पर भगवान् तो उसके इन सब साधनों को जुटाने के माध्यम ही हैं। इसीलिए गीता में भगवान् कहते हैं कि चार प्रकार के मनुष्य मुझे भजते हैं - आर्त्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात् वे जो कष्ट में हों, वे जो संसार में लाभ की खोज करते हों, वे जिनको भगवान् को जानने की जिज्ञासा हो, और वे जिन्हें कि आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया हो। इनमें से ज्ञानी को भगवान् स्वयं अपना स्वरूप हो बताते हैं। वही भगवान् को उनके अपने लिए भजता है बाकी तो सभी किसी न किसी निहित हेतु के लिए भगवान् की ओर जाते हैं। श्रीअरविन्द के निम्न वचन इस पूरे विषय को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकाश में ले आते हैं, "...योग का उद्देश्य है भागवत् उपस्थिति एवं चेतना में प्रवेश करना तथा उसके द्वारा अधिग्रहीत हो जाना, केवल भगवान् के लिए ही भगवान् से प्रेम करना, अपनी प्रकृति में भगवान् की प्रकृति से समस्वर होना तथा अपनी इच्छाशक्ति, क्रिया-कलापों तथा जीवन में भगवान् का यंत्र होना। इसका उद्देश्य कोई महान् योगी या अतिमानव होना (यद्यपि यह हो सकता है) या फिर अहम् की शक्ति, अभिमान या तुष्टि के लिए भगवान् को जकड़ना नहीं है। यह मोक्ष के लिए नहीं है यद्यपि इससे मुक्ति प्राप्त होती है और अन्य सभी वस्तुएँ इससे प्राप्त हो सकती हैं, किंतु ये हमारे उद्देश्य नहीं होने चाहिये। एकमात्र भगवान् ही हमारा उद्देश्य है।" (CWSA 29, p. 21)
"निश्चय ही भगवान् को केवल इसलिए खोजना कि 'उनसे' व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है, सही मनोभाव नहीं है; परंतु यदि 'उन्हें' इन चीजों के लिए खोजना सर्वथा वर्जित होता तो संसार में अधिकांश लोग 'उनकी' ओर बिल्कुल भी अभिमुख नहीं होते। मेरे विचार से यह इसलिए स्वीकार्य है ताकि वे एक आरंभ कर सकें - यदि उनमें श्रद्धा है तो उन्हें उस सब की प्राप्ति हो सकती है जिसकी वे माँग करते हैं और ऐसा करते रहने को अच्छी चीज मानते हैं, और तब सहसा किसी दिन संयोगवश वे इस विचार पर आ सकते हैं कि अंततः यही एकमात्र करने योग्य वस्तु नहीं है, और भी श्रेष्ठतर तरीके व भाव हैं जिनके द्वारा व्यक्ति भगवान् की ओर उन्मुख हो सकता है।" (CWSA 29, p. 8)
व्यक्ति में जो चैत्य सत्ता है वह तो भगवान् की ओर वैसे ही खिंची चली जाती है जैसे नदी सागर की ओर, लोहा चुंबक की ओर तथा पतंगा लौ की ओर चलता है। उसे कोई लाभ-हानि का विचार नहीं रहता। चैत्य के अतिरिक्त अन्य भागों में तो सदा ही अपना कोई निहित हेतु छिपा होता है। यदि व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से अपने आप को अपने इष्ट को दे देने का विचार आता भी है तो उसके पीछे कोई लाभ या प्रतिफल की आशा न्यूनाधिक सूक्ष्म रूप से अवश्य छिपी होती है। इसलिए सूक्ष्म रूप से भी जब तक इस प्रकार का कोई निहित हेतु या कोई प्रतिफल की आशा छिपी होती है तब तक भगवान् में हमारा प्रवेश निषिद्ध है। चैत्य के अतिरिक्त अन्य किसी भाग के द्वारा इस प्रत्याशा को नहीं मिटाया जा सकता। केवल वही है जो भगवान् की ओर जाए बिना रह ही नहीं सकता। उसे इसकी कोई परवाह नहीं कि उससे उसे लाभ होगा या हानि होगी, या फिर भले उसका सर्वनाश ही क्यों न हो जाए। जिसके अंदर यह भाव उदित हो जाता है ऐसा व्यक्ति साधु मानने योग्य है। इसीलिये अपनी शिक्षा की परिणति के रूप में गीता में भगवान् कहते हैं कि सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा।
मीरा बाई के प्रसंग में आता है कि उनके पति भोजराज एक बहुत ही भले व्यक्ति थे। उन्होंने मीरा बाई से कहा कि उन्हें उनके भजन-कीर्तन से कोई आपत्ति नहीं है बस वे केवल इतनी अनुमति चाहते हैं कि वे भी उनके भजन सुन सकें जिससे कि उनका भी कल्याण हो जाए। अब राजा सारे दिन राज-काज संभालते थे और देर रात को भजन सुनते थे। तब मीरा बाई को यह महसूस हुआ कि इतना कार्य करने के बाद रात को जागकर भजन सुनना तो इनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। अतः उन्होंने तय किया कि वे एक निश्चित समय अपना गाना बंद करके अपने कक्ष में जाकर विश्राम करेंगी ताकि राजा भी समय से विश्राम कर सकें। इसलिए मीरा बाई ने अपने तय समय के अनुसार भजन गाना बन्द कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गईं। परंतु तभी उन्हें श्रीकृष्ण की मुरली सुनाई दी और उन्होंने पुनः अवश रूप hat H भजन गाना शुरू कर दिया। सारी योजनाएँ, नियम आदि सब बह गए। इसीलिए श्रीकृष्णप्रेम कहते थे कि श्रीकृष्ण जहाँ छू देते हैं वहीं उन्मत्त कर देते हैं। उनके स्पर्श के बाद व्यक्ति के सभी नैतिक आदर्श, शिष्टाचार-लोकाचार आदि के सभी नियम तो बह जाते हैं।
ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।। १२ ।।
१२. जो भाव हैं (प्रकृति के आत्मपरक रूप हैं), जो कि सात्त्विक, राजसिक और तामसिक हैं, वे मेरे से ही हैं; किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, वे ही मुझमें हैं।
निःसंदेह यहाँ यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पर सूक्ष्म भेद है। भगवान् कहते हैं, "मैं मूलभूत ज्योति, बल, कामना, शक्ति, बुद्धि हूँ पर उनसे उत्पन्न होनेवाले ये विकार मैं निज स्वरूप में नहीं हूँ न उनमें मैं रहता हूँ परन्तु फिर भी ये सब मुझ से ही हैं और सभी मेरी ही सत्ता के अन्दर हैं।"... इस कथन का क्या अभिप्राय है कि भगवान् भूतों में, अपरा प्रकृति के रूपों और भावों में, सात्त्विक भावों तक में नहीं हैं, यद्यपि वे सब हैं उन्हीं की सत्ता के अन्दर? एक अर्थ में तो स्पष्टतः ही भगवान् उनके अन्दर होने ही चाहिये, अन्यथा वे अस्तित्वमान ही नहीं रह सकते। किंतु अभिप्राय यह है कि भगवान् की वास्तविक परम् आत्मप्रकृति उनके अन्दर कैद नहीं है; ये सब उन्हीं की सत्ता में आभास होने वाली चीजें हैं जो कि उस सत्ता में से अहंकार और अज्ञान की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती हैं। अज्ञान हमें सभी चीजों को उल्टा करके प्रस्तुत करता है और कम-से-कम एक अंशतः मिथ्या अनुभूति देता है। हम लोग कल्पना करते हैं कि जीव इस शरीर के अन्दर है, शरीर का ही एक परिणाम और उसी से व्युत्पन्न है; ऐसा ही हम उसे अनुभव भी करते हैं: पर सच तो यह है कि शरीर ही है जो जीव के अंदर है और वही जीव का परिणाम और उससे व्युत्पन्न है। हम अपनी आत्मा को अपने इस महान् अन्नमय और मनोमय व्यापार का एक अंश-सा जानते 8 - 469 जो अंगूठे से बड़ा नहीं है - जबकि वास्तव में यह सारा जगद्व्यापार चाहे जितना भी बड़ा क्यों न प्रतीत होता हो, यह आत्मा की अनन्त सत्ता के अन्दर एक बहुत छोटी-सी चीज है। यहाँ भी यही बात है; उसी अर्थ में ये सब चीजें भगवान् के अन्दर हैं न कि भगवान् उनके अन्दर हैं।
शरीरबद्ध चेतना के अंदर निवास करने के कारण हमें यह आभास होता है कि जड़तत्त्व के अंदर प्राण है और मन है। जबकि वास्तव में तो प्राणमय जगत् तो पूरे जड़ जगत् से अतिविशाल है। इसे एक रूपक के रूप में समझाते हुए हमारे पुराण इसे शेषनाग के हजार फणों के ऊपर एक सरसों के दाने के बराबर बताते हैं। और प्राणमय से मनोमय लोक अतिविशाल है और उससे विज्ञानमय लोक तो अनंततः विशाल है। और फिर आत्मा उससे भी अत्यधिक विशाल है। यह तो केवल सूक्ष्म शरीर की घनीभूत चेतना है जिसके कारण हमें ऐसा विपरीत भ्रम हो जाता है। और स्वयं सूक्ष्म शरीर भी स्थूल देह से अधिक विशाल है।
त्रिभिर्गुणमयैभवैिरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ।। १३ ।।
१३. इन तीन प्रकार के भावों से, जो कि गुणमय हैं, यह संपूर्ण जगत् मोहग्रस्त है और उनसे परे मुझे परम् और अविनाशी के रूप में नहीं जानता।
यह त्रिगुणात्मिका निम्न प्रकृति जो पदार्थों को मिथ्या रूप में दिखाती है और उन्हें निम्नतर रूप दे देती है, माया है। माया से यह तात्पर्य नहीं कि वह कुछ है ही नहीं या वह अयथार्थताओं से अभिप्राय रखती है अपितु इसका यह तात्पर्य है कि यह हमारे ज्ञान को भरमा देती है, झूठे मूल्यों का निर्माण करती है और हमें अहंकार, मानसिकता, इन्द्रिय, दैहिकता और सीमित बुद्धि से आच्छादित कर देती है और इस तरह वहाँ हमसे हमारी सत्ता के परम् सत्य को छिपाये रहती है। यह भ्रमात्मक माया हमसे उस भगवत्स्वरूप को छिपाती है जो हम हैं, अर्थात् अनन्त अक्षर आत्मस्वरूप। ... यदि हम यह देख पाते कि वही भगवत्स्वरूप हमारी सत्ता का यथार्थ सत्य है तो और सब कुछ भी हमारी दृष्टि में बदल जायेगा, अपने सच्चे स्वरूप में आ जायेगा और हमारा जीवन तथा कर्म भागवत् मूल्यों को प्राप्त कर भागवती प्रकृति के विधान के अनुरूप चलेंगे।
यदि हम इसे श्रीअरविन्द की शब्दावली के अनुसार देख पाएँ कि जिसे हम भौतिक शरीर कहते हैं उसमें प्राण के प्रवेश के कारण ही व्यक्ति जीवित रह सकता है। अब भौतिक शरीर के विषय में हमारी अपनी धारणाएँ हैं, उसे देखने के तौर-तरीके हैं। उसके प्रति हम सबके अंदर एक आम दृष्टिकोण है कि अमुक चीज करने से ऐसा या वैसा हो जाता है और यह दृष्टिकोण हम सबमें अंतर्निहित है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इन धारणाओं को अनदेखा कर सकता हो। हम उनसे बँधे हुए हैं। इसे हम तामसिक क्रिया-कलाप कह सकते हैं। जब इस अवस्था में प्राणिक प्रकृति का संचार होता है तब दूसरों के प्रति संवेदनाएँ, भावनाएँ आदि आती हैं जो घोर भौतिक विषयों से कुछ मुक्त करती हैं। किसी दूसरे के प्रति अपनी भावना के सहारे व्यक्ति अपने भौतिक सुख-आराम को भी बहुत कुछ छोड़ सकता है क्योंकि अब उसे तामसिक की बजाय राजसिक तुष्टि प्राप्त होती है। जब राजसिकता आती है तब व्यक्ति किन्हीं भी अभियानों को हाथ में लेने से या किन्हीं श्रमसाध्य कार्यों को करने से नहीं हिचकिचाता जबकि एक तामसिक व्यक्ति कभी नए अभियानों को नहीं करना चाहता और सदा ही अपने सुख-चैन के दायरे में निश्चिंत रूप से रहना चाहता है। यदि यह राजसिक तत्त्व न होता तो संसार में कोई भी नवीन चीजें आ ही नहीं सकती थीं। सत्त्व प्रधान व्यक्ति सभी चीजों के सही विधान को खोजने का प्रयास करता है। वह अपनी निरंकुश प्राणिक प्रकृति पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है और जो सही है वही करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों ही गुण होते हैं, भेद केवल इनके प्राधान्य का रहता है। जिस तत्त्व का प्राधान्य होता है उसी के अनुसार हम उस व्यक्ति को सात्त्विक, राजसिक या तामसिक बता देते हैं। इस प्रकार ये तीनों ही गुण मनुष्य जीवन का ताना-बाना बुनते हैं और व्यक्ति प्रायः इनसे ऊपर नहीं उठ पाता क्योंकि यह ताना-बाना उसे बिल्कुल वास्तविक लगने लगता है। जहाँ तामसिक और राजसिक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुचित होने का भान हो सकता है वहीं सात्त्विक व्यक्ति tilde H तो अपने सही होने का अहंकार उत्पन्न होने की बहुत आशंका रहती है। परन्तु तीनों ही गुणों का यह सारा ताना-बाना माया ही है। परंतु सत्त्व प्रधान व्यक्ति में सामंजस्य अधिक होता है जिससे कि आत्मा को क्रिया करने की अधिक संभावना मिल जाती है। हालाँकि यदि भीतर आत्मा प्रबल हो तो वह किसी भी अवस्था से बंधनों को तोड़कर बाहर आ सकती है। परंतु गीता का क्रम एक सर्वसामान्य क्रम है जिसमें तीनों गुणों का व्यापार चलता रहता है और धीरे-धीरे व्यक्ति सात्त्विकता की ओर बढ़ता रहता है। परंतु यह सारा ही व्यापार माया है।
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।। १४ ।।
१४. यह मेरी गुणात्मिका दैवी माया है जिसे अतिक्रम करना कठिन है; जो मनुष्य मेरी ओर मुड़ते हैं और मेरे समीप आते हैं, केवल वे ही इस माया को पार करते हैं।
पर जब भगवान् ही इन सब चीजों में हैं और भागवती प्रकृति ही इन सब भरमानेवाले विकारों के मूल में भी विद्यमान है और जब हम सब जीव हैं और जीव वही भागवती प्रकृति है तब क्या कारण है कि इस माया को पार करना इतना कठिन है, 'माया दुरत्यया'? क्योंकि यह माया भी तो भगवान् की माया है, 'दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया' अर्थात् 'यह गुणमयी दैवी माया मेरी है'। यह स्वयं दैवी है और भगवान् की ही प्रकृति की उपज है, किन्तु अवश्य ही देवताओं के रूप में भगवान् की प्रकृति की उपज है; यह दैवी है, अर्थात् देवताओं की है या यह कहिये कि देवाधिदेव की है, परन्तु देवाधिदेव के अपने विभक्त आत्मनिष्ठ तथा निम्न वैश्व भावों अर्थात् सात्त्विक, राजसिक, और तामसिक भाव की चीज है। यह एक वैश्व आवरण है जो देवाधिदेव ने हमारी बुद्धि के चारों ओर बुन रखा है; ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ने इसके जटिल ताने-बाने बुने हैं; पराप्रकृतिरूपिणी शक्ति इस बुनावट के मूल में है और इसके प्रत्येक तंतु में छिपी हुई है। हमें इस बुनावट को अपने अन्दर पूरा करना है और जब इसका उपयोग समाप्त हो जाए तो इसमें से हो कर, इसे पीछे छोड़ आगे बढ़ना है, देवताओं से हटकर उन परम् आदिस्वरूप देवाधिदेव की ओर मुड़ना है जिनमें हम देवताओं और उनके कर्मों का परम् अभिप्राय तथा स्वयं अपनी ही अक्षर आत्म सत्ता के परम् गुह्य आध्यात्मिक सत्यों को एक ही साथ जान जाएँगे।
इन तीनों गुणों ने अपना ताना-बाना बुन रखा है जिन्हें लाँघकर व्यक्ति को अपनी सच्ची प्रकृति में जाना होगा। परन्तु यह साधित कैसे हो इसका निरूपण अब होगा कि जब व्यक्ति भगवान् की ओर मुड़ता है तब ज्ञान भक्ति में परिणत हो जाता है और ज्ञान तथा भक्ति का समन्वय हो जाता है। ज्ञान की परिसमाप्ति भक्ति में होती है और उसी से सच्चे कर्मों का आरम्भ होता है। बिना भगवान् की भक्ति के सच्चे कर्म हो ही नहीं सकते।
II. भक्ति और ज्ञान का समन्वय
गीता ... इस अध्याय के पहले चौदह श्लोकों में एक ऐसे प्रमुख दार्शनिक सत्य को प्रदान कर, जिसे जानने की हमें आवश्यकता है, तुरंत ही बाद के सोलह श्लोकों में उसका व्यावहारिक प्रयोग करती है। वह इस ज्ञान को कर्म, ज्ञान और भक्ति के एकीकरण के प्रथम प्रारंभ-बिंदु में बदल देती है, - क्योंकि कर्म और ज्ञान का प्राथमिक समन्वय इनके द्वारा अपने-आप में तो पहले ही साधित किया जा चुका है।
.... परा-प्रकृति क्रिया के लिए, प्रवृत्ति के लिए, बहुरूप आत्म-व्यक्तित्व या जीव बनती है। परन्तु इस परा-प्रकृति का आन्तरिक या वास्तविक कार्य सदा ही एक आध्यात्मिक, एक भागवत् क्रिया होती है। इस परा भागवती प्रकृति की शक्ति ही अर्थात् परम् पुरुष की सत्ता की चिन्मयी संकल्पशक्ति ही जीव के विशेष गुण की विविध बीजभूत और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अपने-आप को प्रकट करती है; यही बीजभूत शक्ति जीव का स्वभाव है। इस आध्यात्मिक शक्ति से ही सीधे जो कर्म और जन्म होता है वह दिव्य जन्म और विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म होता है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकला कि कर्म करते हुए जीव का यही प्रयास होना चाहिये कि वह अपने मूल आध्यात्मिक व्यष्टि-स्वरूप को प्राप्त हो और अपने कर्मों को उसी की परमा शक्ति के ओज से प्रवाहित करे, कर्म को अपनी अंतरात्मा और अंतरतम स्वरूप-शक्ति से विकसित करे, न कि मन-बुद्धि की कल्पना और प्राणों की इच्छा से, और इस तरह अपने सब कर्मों को परम् पुरुष के संकल्प का ही विशुद्ध प्रवाह बना दे, अपने सारे जीवन को भागवत्-स्वभाव का गतिशील प्रतीक बना दे।
परन्तु इसके साथ ही यह त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति भी है जिसका स्वभाव अज्ञान का स्वभाव है और उसका कर्म अज्ञान का कर्म है, मिलावटी है, भ्रांत है और विकृत है; यह निम्नतर व्यक्तित्व का, अहंकार का, प्राकृत पुरुष का कर्म होता है, आध्यात्मिक व्यष्टि-पुरुष का नहीं। उस मिथ्या व्यक्तित्व से दूर होने के लिए हमें निर्वैयक्तिक आत्मा की शरण लेकर उसके साथ एक हो जाना होता है। तब, इस प्रकार अहंकारमय व्यक्तित्व से मुक्त होकर, हमारे वास्तविक व्यष्टि-स्वरूप का पुरुषोत्तम के साथ जो संबंध है उसे हम जान सकते हैं।
इस टीका से प्रकट होता है कि अपरा प्रकृति भी परा प्रकृति का ही रूप है परन्तु जब व्यक्ति सतही प्रकृति पर, अपने अहं पर ही केन्द्रित होता है तब प्रकृति की जैसी क्रिया होती है वह दिखने में अज्ञानमय और सीमित तरीके की होती है क्योंकि मनुष्य को उस स्तर से ऊपर उठाने के लिये तब वही आवश्यक होती है। इसे हम अपरा प्रकृति का नाम दे देते हैं। इसके चंगुल से निकलने के लिये गीता जो उपाय बताती है, जो कि बहुत से लोगों के लिये बहुत उपयोगी है, वह है निर्वैयक्तिक हो जाना, अर्थात्, अक्षर पुरुष से तादात्म्य स्थापित करना। क्योंकि वैयक्तिकता में, अर्थात्, क्षर सत्ता में भौतिक, प्राणिक, मानसिक आदि की बाधाएँ आती हैं। और अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के पश्चात् पुरुषोत्तम भाव की ओर जाना होता है क्योंकि भगवान् कहते हैं कि वे उस अक्षर भाव से भी परे हैं।
एक दृष्टिकोण से देखें तो यह सारा क्रिया-कलाप परम प्रभु की परम शक्ति, परा-प्रकृति, आद्या-शक्ति, माँ भगवती का ही है। जब मनुष्य जड़-भौतिक चेतना में निवास करता है तब उसे परिचालित करने के लिए वे भौतिक नियमों आदि का उपयोग करती हैं। वास्तव में तो सर्वत्र उन्हीं का संकल्प पूरा होता है जिसके अतिरिक्त अन्य कोई नियम-विधान नहीं है। परंतु इस प्रकार की क्रमविकासमय सृष्टि का निर्माण करने के लिए, जहाँ सभी चीजें एक सही व्यवस्था के अनुसार चलें, आत्मा की शक्ति, जिसे कि वेदों में बृहस्पति कहा गया है, के द्वारा विभिन्न स्तरों का और उनमें निश्चित निर्धारित तौर तरीकों का निर्माण किया जाता है ताकि यज्ञ के आरोहण के लिए यज्ञीय भूमि तैयार की जा सके। यदि इन स्तरों में अपने-अपने उचित नियम-विधान न हों तो बिल्कुल विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी और किसी प्रकार का यज्ञ संपन्न ही नहीं हो पाएगा। आरंभ में तो इस आत्मा की शक्ति के द्वारा निश्चेतना (nescience), जो कि चेतना का बिल्कुल निषेध है और जहाँ शून्यता तक के लिए भी कोई स्थान नहीं है, के अंदर से इस जड़-भौतिक तत्त्व का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यह सारी सृष्टि परा प्रकृति के द्वारा ही की जाती है और सारे नियम-विधान भी आत्मा की शक्ति के द्वारा ही लागू किये जाते हैं जबकि वास्तव में अपने आप में कोई नियम नहीं हैं। और जब सभी कुछ एक ही है तो भिन्न-भिन्न चीजें तो हैं ही नहीं। केवल मानसिक निरूपण के लिए हम भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। और श्रीअरविन्द भी गीता पर टीका करने के कारण गीता की ही शब्दावली का प्रयोग करते हैं।
परंतु वर्तमान में इस त्रिगुणमयी प्रकृति से निकल कर उच्चतर प्रकृति में जाने के लिए हमें स्वयं को सभी कर्मों से अलग हटकर साक्षी भाव में और उसके बाद पुरुषोत्तम भाव में जाना होगा। गीता में प्रतिपादित यह एक तरीका है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से तरीके हो सकते हैं। श्रीमाँ व श्रीअरविन्द का योग भी इस पद्धति से भिन्न है। परंतु गीता के निरूपण के समय यह प्रचलित तरीका था और अर्जुन उससे अभिज्ञ था इसलिए गीता इस पद्धति का प्रतिपादन करती है। हालाँकि ये सभी प्रतिपादन करने के बाद अंत में गीता सभी धर्मों (आधारों) को छोड़ कर एकमात्र भगवान् की शरण में आने की बात करती है। और यही पूर्ण समर्पण का भाव श्रीअरविन्द के अतिमानसिक योग का मूल तत्त्व है। गीता अपनी शिक्षा को यहीं लाकर छोड़ देती है और इससे आगे निरूपण नहीं करती क्योंकि इसके आगे तो अनुभव ही करना होता है। हालाँकि उससे आगे के पथ-संकेत भी हमें श्रीअरविन्द व श्रीमाँ की कृतियों से प्राप्त होते हैं।
अब यहाँ गीता में पहली बार हम आसुरिक स्वभाव का वर्णन पाते हैं। बाद में देव और असुर का अन्तर भी स्पष्ट किया जाएगा। भगवान् कहते हैं कि आसुरिक प्रकृति वाले लोग उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। और दैविक प्रकृति के लोगों के चार भेद हैं जिन्हें अपने-अपने तरीके से भिन्न फल प्राप्त होते हैं। यह आसुरिक और दैविक प्रकृति सब मनुष्यों में होती है। परन्तु गीता जो बात कर रही है वह एक मूलभूत आसुरिक प्रकृति और दैविक प्रकृति की बात है। जो अपने मूल गठन मात्र में ही आसुरिक प्रकृति वाला है वह भगवान् की ओर नहीं जा सकता। श्रीअरविन्द इसके बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि ये सत्ताएँ धरती की नहीं होतीं बल्कि सूक्ष्म जगतों की होती हैं और वहाँ से अपना प्रभाव डालती हैं जो कि तीन तरीकों का होता है। पहले तो ये शक्तियाँ आक्रमण करती हैं। यह तो एक बहुत ही आम घटना है जो लगभग सभी के साथ होती है और जहाँ भागवत् कार्य हो रहा हो वहाँ तो इनके आक्रमण अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। परंतु इन आक्रमणों के प्रभाव से कुछ समय के बाद व्यक्ति के बाहर निकल आने की संभावना रहती है। इससे अधिक गंभीर होता है इन शक्तियों द्वारा मनुष्य पर अपना प्रभाव छोड़ना। एक बार इनसे प्रभावित होने पर मनुष्य के मन, प्राण, विचार, दृष्टिकोण आदि सभी चीजें प्रभावित हो जाती हैं और उनके संतुलन को पुनः स्थापित करना मुश्किल होता है। परंतु सबसे भयंकर स्थिति है इन शक्तियों द्वारा पूरी तरह अधिकृत किये जाना। जब ये व्यक्ति पर अपना अधिकार जमा लेती हैं तब वह उनके वश में हो जाता है और इसकी पूरी आशंका होती है कि वे उसके चैत्य पुरुष को पूरी तरह निष्कासित कर दें और तब वह आसुरी शक्तियों द्वारा एक पूर्ण अधिग्रहण हो जाता है। हालाँकि बहुत ही विरले मामलों में ऐसा होता है।
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ।। १५।।
१५. दुष्कर्म करनेवाले मोहग्रस्त निम्न श्रेणी के मनुष्य मुझे नहीं प्राप्त होते; क्योंकि उनका ज्ञान उनसे माया के द्वारा हरण किया जा चुका होता है और वे आसुरिक भाव का आश्रय ग्रहण करते हैं।
यह मूढ़ता प्रकृतिस्थ जीव को भ्रामक अहंकार द्वारा धोखा दिया जाना है। दुष्कर्मी परम् पुरुष को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वह सदा ही मानव-प्रकृति के निम्नतम स्तर पर अपने इस इष्टदेव अहंकार को ही तुष्ट करने का प्रयास करता रहता है; उसका वास्तविक परमेश्वर यह अहंकार ही होता है। उसके मन और संकल्प, जो त्रिगुणात्मिका माया की क्रियाओं द्वारा घसीट ले जाए जाते हैं, आत्मा का उपकरण नहीं रह जाते अपितु उसकी कामनाओं के, स्वेच्छा से गुलाम या अपने-आप को धोखा दिये हुए यंत्र बन जाते हैं। तब वह केवल इस निम्न प्रकृति को ही देखता है और अपने उस परम् आत्मतत्त्व को तथा परम् पुरुष या परमेश्वर को नहीं देखता जो उसके स्वयं के और जगत् के अन्दर है; वह अपने मन में सारे जगत् की व्याख्या अहंकार और कामना के अर्थों में करता है और केवल अहंकार और कामना को ही पुष्ट करता है। किसी उच्चतर प्रकृति और किसी उच्चतर धर्म से रहित होकर, अहंकार और कामना की सेवा करना असुर के मन और स्वभाव को प्राप्त करना है। ऊपर उठने के लिए प्रथम आवश्यक सोपान है उच्चतर प्रकृति और उच्चतर धर्म के लिए अभीप्सा करना, कामना के शासन की अपेक्षा किसी महत्तर विधान की पालना करना, और अहंकार या अहंकार के किसी परिवर्धित रूप की अपेक्षा किसी श्रेष्ठतर देवता का बोध करना और उसे पूजना, सद्विचार से युक्त होना और सत्कर्मी बनना। यह भी अपने-आप में पर्याप्त नहीं है; क्योंकि सात्त्विक मनुष्य भी गुणों के संभ्रम के अधीन होता है, क्योंकि अब भी वह इच्छा (राग) और द्वेष के द्वारा ही चालित होता है। वह प्रकृति के नाना रूपों के चक्र के अंदर ही घूमता रहता है और उसे उच्चतम, लोकोत्तर और समग्र ज्ञान नहीं होता। तथापि अपने सदाचारी या धर्मपरायण लक्ष्य में सतत् ऊर्ध्वमुखी अभीप्सा के द्वारा वह अन्त में पाप के तमाच्छादन से - जो तमाच्छादन राजसिक कामना तथा आवेगों का परिणाम है, उससे - मुक्त होता है और ऐसी विशुद्ध प्रकृति अर्जित करता है जो त्रिगुणात्मिका माया के अधिकार से मुक्ति पाने में समर्थ होती है। केवल पुण्य के द्वारा ही मनुष्य सर्वोच्च को नहीं पा सकता, परंतु पुण्य के द्वारा वह उसे पाने का पहला सामर्थ्य अर्थात् 'अधिकार' विकसित कर सकता है। क्योंकि अशिष्ट राजसिक या मन्द तामसिक अहंकार को हटा देना और उससे ऊपर उठना कठिन होता है; जबकि सात्त्विक अहंकार को हटाकर उससे ऊपर उठना कम कठिन होता है और अंततः जब वह अपने आप को यथेष्ट रूप से सूक्ष्म और प्रकाशयुक्त बना लेता है, तब उसे अतिक्रम कर जाना, उसे रूपान्तरित करना या मिटा देना भी आसान हो जाता है।
दुष्कर्म करनेवाले, अपनी इच्छाओं-कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोग अपने इष्टदेव अहं को ही पुष्ट करने में लगे रहते हैं। अपने मन, प्राण और शरीर की माँगों को पूरा करने के अतिरिक्त तो उन्हें और कुछ पता हो नहीं होता। परंतु जब व्यक्ति के मन में किसी लोकोत्तर चीज के लिये अभीप्सा जागृत होती है और वह अपनी मानसिक, प्राणिक और शारीरिक कामनाओं के स्थान पर उस अभीप्सा के अनुसार जीने का प्रयास करता है तब इसका अर्थ है कि वह सही मार्ग पर है। फिर धीरे-धीरे, जैसा कि श्रीअरविन्द बताते हैं कि "केवल पुण्य के द्वारा ही मनुष्य सर्वोच्च को नहीं पा सकता, परंतु पुण्य के द्वारा वह उसे पाने का पहला सामर्थ्य अर्थात् 'अधिकार' विकसित कर सकता है।" अतः वह सत्त्व के द्वारा पूरी तरह मुक्त तो नहीं हो सकता परंतु तामसिक तथा राजसिक स्थिति की अपेक्षा एक बेहतर स्थिति में होता है कि आगे की छलाँग लगा पाए। क्योंकि तामसिक और राजसिक स्थिति से ऊपर उठ पाना बहुत अधिक मुश्किल है जबकि सात्त्विक अवस्था से ऊपर उठना अपेक्षाकृत आसान है। और सात्त्विक अवस्था में व्यक्ति जब धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाता है तब उस अवस्था को पार करके आगे भी जा सकता है। दैवी प्रकृति वाले तमस् प्रधान भी हो सकते हैं और रजस् प्रधान भी। परंतु दैवी प्रकृति का सही प्रस्फुटन सात्त्विक प्रकृति में ही अधिक होता है। तमस् में तो अंधकार की ही संभावना अधिक रहती है। परन्तु यदि व्यक्ति का गठन दैवी प्रकृति का हो तो वह इन निम्नतर रूपों से जल्दी ही ऊपर उठ जाता है। वह सुकृत कर्म करने वाला होता है दुष्कर्म करने वाला नहीं। पर यदि व्यक्ति मूल रूप से आसुरिक प्रकृति का हो तो फिर बाहरी रूप से उसका कितना भी विकास क्यों न हुआ हो तो भी वह रहेगा भगवद्विरोधी ही।
इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम 'सुकृत', अर्थात् सदाचारी होना चाहिए और तब उसे जीने के महज नैतिक विधान से परे की ऊँचाइयों में ऊपर उठकर अध्यात्मप्रकृति के प्रकाश, विशालता और शक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिये... हम पहले ही देख चुके हैं कि इस उद्देश्य के लिए आत्म-ज्ञान, समत्व, निरहंकार प्रथम आवश्यकताएँ हैं, और यह भी देख चुके हैं कि यही ज्ञान और कर्म के बीच, आध्यात्मिकता और सांसारिक कार्य के बीच, कालातीत आत्मा की अचल निष्क्रियता और प्रकृति की क्रियाशील शक्ति की लीला के बीच सामंजस्य साधने का मार्ग है। परंतु गीता अब उस कर्मयोगी के लिए, जिसने अपने कर्म को ज्ञानयोग के साथ एक कर लिया है, एक और, इससे भी बड़ी चीज की आवश्यकता बतलाती है। अब उससे केवल ज्ञान और कर्म की ही नहीं अपितु भक्ति की भी माँग की जाती है, भगवान् की भक्ति, उनसे प्रेम और उनकी आराधना और सर्वोच्च से मिलने की अंतरात्मा की उत्कण्ठा भी चाही जाती है। यह माँग, जो अभी तक उतने स्पष्ट शब्दों में तो नहीं प्रकट की गयी थी, परंतु इसकी तैयारी तभी हो चुकी थी जब श्रीगुरु ने उसके योग के एक आवश्यक मोड़ के रूप में सभी कर्मों को रूपांतरित कर हमारी सत्ता के स्वामी के प्रति यज्ञरूप से किये जाने का प्रतिपादन किया था और इसकी परिणति के रूप में यह नियत किया था कि सब कर्मों को न केवल हमारी निर्वैयक्तिक आत्मा या ब्रह्म को दे देना है अपितु निर्वैयक्तिक आत्मा से परे उन परम्-सत्ता को समर्पित करना होगा जिनसे हमारा सब संकल्प और शक्ति उद्भूत होते हैं। वहाँ जो बात गुप्त रूप से अभिप्रेत थी उसे ही अब सामने लाया गया है और इससे हम गीता के उद्देश्य को और भी अधिक पूर्णता के साथ समझने लगते हैं।...."जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वही संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण भाव के साथ मेरी भक्ति करता है (भजति)।" और संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण आत्म-समर्पण वाली यह भक्ति ही है जिसका अब गीता विस्तार करना आरंभ करती है।
यह बात ध्यान में रहे कि गीता शिष्य से जिस भक्ति की माँग करती है वह ज्ञानयुक्त भक्ति है और भक्ति के अन्य सभी प्रकारों को अपने आप में अच्छा समझते हुए भी ज्ञानयुक्त भक्ति की अपेक्षा निम्न ही मानती है; भक्ति के उन अन्य प्रकारों से लाभ हो सकता है, पर जीव के परमोत्कर्ष में वे गीता के अनन्य लक्ष्य नहीं हैं। जिन लोगों ने राजस् अहंकार के पाप को दूर कर दिया है और जो भगवान् की ओर बढ़ रहे हैं उनमें से गीता ने चार प्रकार के भक्तों में भेद किया है।
रजस् अहंकार अपने निज बल पर भरोसा करता है। उसे यह अहंकार होता है कि वह स्वयं अपनी ही शक्ति-सामर्थ्य से कार्यों को करता है। वहीं भगवान् पर निर्भरता आत्मा का भाव है। अतः जब आस्तिकता आती है तब फिर उस पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारी सत्ता के किसी न किसी भाग में भगवान् पर विश्वास हुए बिना यह संभव नहीं है। तो जो भगवान् की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे चार प्रकार के भक्तों में गीता विभेद करती है। श्रीअरविन्द कहते हैं कि तामसिक, राजसिक, सात्त्विक और निस्त्रैगुण्य, ये भक्ति के चार रूप हैं।
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।। १६ ।।
१६. हे भरतकुलश्रेष्ठ! शुभ कर्म करनेवाले चार प्रकार के मनुष्य मुझे भजते हैं, वे जो कष्ट में हों, वे जो संसार में लाभ की खोज करते हों, वे जो ज्ञान की खोज करते हों, और वे जो ज्ञानी हों।
ये सभी गीता द्वारा स्वीकृत हैं, परंतु केवल अंतिम प्रकार के भक्त पर ही वह अपनी पूर्ण सम्मति की छाप लगाती है। बिना किसी अपवाद के भक्ति के ये सभी प्रकार निश्चय ही उच्च व उत्तम हैं, उदाराः सर्व एवैते, परन्तु ज्ञानयुक्त भक्ति इन सभी से श्रेष्ठ है, विशिष्यते। हम कह सकते हैं कि भक्ति के चार प्रकार क्रमशः ये हैं : (प्रथम) प्राणिक-रागात्मक तथा भावात्मक प्रकृति की भक्ति, (द्वितीय) व्यावहारिक और सक्रिय, कर्म-प्रधान प्रकृति की, (तृतीय) तर्क-प्रधान बौद्धिक प्रकृति की, और (चतुर्थ) उस परम् अंतर्ज्ञानमय सत्ता की भक्ति जो शेष सारी प्रकृति को भगवान् के साथ एकत्व में ले लेती है। भक्ति के अंतिम प्रकार को छोड़ अन्य जितने प्रकार हैं उन्हें वस्तुतः प्रारंभिक प्रयास ही माना जा सकता है। क्योंकि गीता स्वयं यहाँ कहती है कि अनेकों जन्मों के अंत में समग्र ज्ञान को पाकर और उसे अनेकों जन्मों तक अपने जीवन में उतारने का साधन करके सुदीर्घ अन्त में व्यक्ति परात्पर को प्राप्त करता है।
vii. 17, vii. 18
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ।। १७।।
१७. इन (चार प्रकार के भक्तों) में जो भगवान् के साथ सतत् युक्त रहता है, जिसकी भक्ति पूर्ण रूप से भगवान् पर ही केंद्रित है, ऐसा ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। मैं ज्ञानी को परम् प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है।
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ।। १८ ।।
१८. ये सभी उच्च और श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी' को मैं वस्तुतः मेरा निजस्वरूप ही मानता हूँ; क्योंकि मुझमें अपने अंतःकरण को युक्त किया हुआ वह भक्त मुझे ही अपने उच्चतम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है।
गीता अब धीरे-धीरे भक्ति तत्त्व की प्रधानता की ओर मुड़ रही है और कहती है 'उदाराः सर्व एवैते' कि सारे ही भक्त श्रेष्ठ हैं। क्योंकि वास्तव में तो जो भी कोई भगवान् की ओर जिस किसी भी भाव से मुड़ गया है अवश्य ही वह श्रेष्ठ है।
प्रश्न : क्या भगवान् भी इस अहंकार के दृष्टिकोण से देखते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वही मेरे पास आ सकता है?
उत्तर : भगवान् तो परम अहंकारी है। क्योंकि उनके अतिरिक्त अन्य किसी की तो सत्ता है ही नहीं। इसीलिए सभी भक्तों में ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि उसे भगवान् के आत्मस्वरूप का, उनके निजस्वरूप का ज्ञान होता है और साथ ही उसे यह भी ज्ञान होता है कि उसका अपना आत्मस्वरूप भगवान् के साथ अभिन्न है। ज्ञानी के अतिरिक्त दूसरे भक्त तो भगवान् को अपनी सत्ता से भिन्न समझते हैं। परंतु ज्ञानी भगवान् के और अपने सच्चे स्वरूप को जानता है और चूंकि वह सच्चे स्वरूप को जानता है इसलिए सहज रूप से ही वह भगवान् की भक्ति करता है क्योंकि तत्त्वतः जानने के बाद दूसरा कोई भाव तो हो ही नहीं सकता। और भले कोई तथाकथित रूप से बहुत ही ज्ञानी हो पर भगवान् की ओर अभिमुख नहीं हो तो वह ज्ञानी नहीं महामूर्ख है। अब रावण में भले ही कितना भी पांडित्य क्यों न रहा हो, परंतु वह किस काम का। इसीलिए हनुमानजी उसे कहते हैं :
राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई।।
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरषि गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं ।।
अर्थात् जैसे जिन नदियों के मूल में कोई जलस्रोत नहीं है वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं ठीक उसी प्रकार राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है क्योंकि इन सबका मूल स्रोत तो श्रीराम ही हैं।
प्रायः ही हमारी समझदारी और नासमझी की सारी परिभाषाएँ बिल्कुल दकियानूसी होती हैं। जो भगवान् की ओर अभिमुख है वही सच्चा समझदार है, वहीं, जो बाहर से बहुत कुशल है और बहुत से हुनर जानता है पर यदि भगवान् से विमुख है तो वह महामूर्ख है।
---------------------------
...जब ईश्वरप्रेमी ईश्वरज्ञानी भी हो, तो प्रेमी अपने दिव्य प्रियतम के साथ एकात्म हो जाता है; क्योंकि वह परमोच्च देव का चुना हुआ और परमात्मा का वरण किया हुआ होता है। अपने अंदर इस भगवत्-लीन प्रेम को विकसित करो; आध्यात्मीकृत और अपनी निम्न प्रकृति की सीमाओं के ऊपर उठा हुआ हृदय तुम्हें परमेश्वर की अमित सत्ता के रहस्य अत्यंत अंतरंग रूप में प्रकाशित कर देगा, उनकी दिव्य शक्ति के पूर्ण संस्पर्श को, प्रवाह को और महिमा को तुम्हारे अंदर ले आएगा और तुम्हारे लिए एक शाश्वत परमोल्लास के गुह्य रहस्यों को खोल देगा। पूर्ण प्रेम ही पूर्ण ज्ञान की कुंजी है।
गीता भक्ति के तीन प्रकारों में भेद करती है, एक वह जो संसार के दुःखों के कारण भगवान् की शरण लेती है, आर्ता, दूसरी वह जो किसी चीज की कामना करती हुई, इष्टफलदाता के रूप में भगवान् के पास जाती है, अर्थार्थी; और तीसरी वह है जो उसके द्वारा आकृष्ट होती है जिसे वह प्रेम तो पहले से ही करती है परंतु उसे अभी तक जानती नहीं है और इस दिव्य अज्ञात को जानने के लिए आतुर है, जिज्ञासुः परन्तु यह परम् श्रेय उस भक्ति को देती है जो ज्ञानयुक्त हो। स्पष्ट ही, भाव की जो तीव्रता ऐसा कहती हो कि, "मैं समझती तो नहीं, मैं प्रेम करती हूँ", और, प्रेम करती हुई, समझने की परवाह भी नहीं करती, तो वह प्रेम की अन्तिम नहीं, अपितु प्रथम आत्म-अभिव्यक्ति है, और न ही वह उसकी उच्चतम तीव्रता ही है। वास्तव में, जैसे-जैसे भगवान् का ज्ञान विकसित होता है, वैसे-वैसे भगवान् में आनन्द और उससे प्रेम भी बढ़ता ही है। और फिर, ज्ञान के आधार के बिना निरा आनन्दातिशय सुरक्षित भी नहीं रह सकता; जिससे हम प्रेम करते हैं उसी में निवास करना ही वह सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें निवास करने का अर्थ है चेतना में उसके साथ एक होना, चेतना का एकत्व ही ज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था है। भगवान् का ज्ञान भगवत्प्रेम को उसकी सुदृढ़तम सुरक्षा प्रदान करता है, इसके लिए इसके स्वयं के अनुभवजन्य विपुलतम हर्ष को खोल देता है, इसे इसके दृष्टिविस्तार के उच्चतम शिखरों तक उठा देता है।
अगला श्लोक भी बड़ा ही मार्मिक है। जो ज्ञानी यह जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है।
प्रश्न : पंद्रहवें अध्याय में श्लोक आता है : यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ।। १९।।
अर्थात्, 'हे भारत! मोहरहित जो मनुष्य इस प्रकार मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता एवं देखता है वह सर्व-ज्ञाता अपनी प्राकृत सत्ता के हर रूप, हर प्रकार से मेरी भक्ति करता है।' तो क्या यह बाध्यता है कि जो पुरुषोत्तम के रूप को जान लेता है उसे सर्वभाव से उन्हें भजना ही होता है?
उत्तर : इसमें बाध्यता की बात नहीं भाव की बात है क्योंकि वास्तव में परमात्मा का स्वरूप जानने के बाद व्यक्ति अनायास ही और कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि अब उसकी चेतना इतनी विकसित हो चुकी होती है कि वह कुछ और चाह ही नहीं सकता। यहाँ ज्ञान-युक्त भक्ति की बात कर रहें है। और गीता कहती है कि जिसे ज्ञान हो गया है ऐसे भक्त को भी अनेक जन्मों के बाद भगवान् प्राप्त होते हैं।
प्रश्न : क्या इसका तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञानवान् होने के लिये बहुत से जन्मों की आवश्यकता है?
उत्तर : नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानवान् होने के बाद भी बहुत से जन्मों की आवश्यकता होती है। ज्ञान होने पर व्यक्ति को अपने सच्चे गंतव्य का पता लग जाता है। और जब एक बार गंतव्य का पता लग जाता है तब उस ओर चलकर वहाँ पहुँचने में जो समय लगता है उतना तो लगता ही है। इसीलिए ज्ञानवान् व्यक्ति भी बहुत से जन्मों के अंत में भगवान् को प्राप्त करता है। पहले तो व्यक्ति को यह पता होना आवश्यक है कि वह कौन है, और उसका उद्देश्य क्या है, और उसे कहाँ जाना है। जब एक बार इन प्रश्नों का किसी स्तर तक उत्तर मिल जाता है तब कार्य समाप्त नहीं हो जाता बल्कि वास्तव में कार्य तो आरंभ ही उस ज्ञान के बाद होता है। और तब उसे संसिद्ध करने में जितना समय लगता है वह तो लगता ही है। अन्यथा अधिकांशतः तो कोई यह प्रश्न भी नहीं पूछता कि पार्थिव जन्म का कोई अर्थ भी है। और यदि अर्थ है भी तो उसे कैसे खोजा जाए और कैसे प्राप्त किया जाए। केवल भारतीय संस्कृति ने ही न केवल इन प्रश्नों को सफल रूप से हाथ में लिया अपितु प्रत्येक व्यक्ति को उसके जिस किसी भी स्तर से शीघ्रातिशीघ्र अपने सच्चे गंतव्य तक पहुँचने में सहायता प्रदान करने की समुचित व्यवस्था भी की।
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।। १९।।
१९. बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानवान् व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है; और वह यह देखता है कि जो कुछ भी है वह सब कुछ सर्वव्यापी सत्ता भगवान् वासुदेव ही हैं। ऐसी महान् आत्मा अति दुर्लभ है।
सभी वस्तुओं की ईश्वर या ब्रह्म के रूप में इस अनुभूति के तीन पहलू हैं जिनकी कि हम सुविधापूर्वक अनुभव की तीन क्रमिक अवस्थाएँ बना सकते हैं। प्रथम अनुभूति यह कि, एक विराट् आत्मा है जिसमें सब प्राणी अस्तित्वमान रहते हैं। आत्मा एवं भगवान् ने स्वयं को एक ऐसी अनन्त स्वतः-व्याप्त, स्वयंभू, शुद्ध सत्ता के रूप में अभिव्यक्त किया है जो देश और काल के अधीन नहीं है, अपितु इन्हें अपनी चेतना की आकृतियों के रूप में धारण करती है। वह सभी वस्तुओं से विशाल है और इन सबको अपनी स्वतःव्याप्त सत्ता और चेतना में समाविष्ट किये हुए है। जिन भी चीजों को वह रचती है, धारण करती है या जिन भी चीजों का रूप ग्रहण करती है उनमें से किसी से भी वह बंधी हुई नहीं है, अपितु मुक्त, अनन्त और सर्वानन्दमय है। एक प्राचीन रूपक के शब्दों में, वह उन्हें उसी प्रकार धारण करती है जिस प्रकार अनन्त आकाश अपने अन्दर सब पदार्थों को धारण करता है... [और आत्मतत्त्व या ब्रह्म में समाहित ये सभी पदार्थ] शून्य नहीं हैं, विराट् मन के द्वारा कल्पित मिथ्या नाम-रूपमात्र नहीं हैं; ... ये अपने वास्तविक रूप में आत्मतत्त्व की सचेतन अभिव्यक्तियाँ हैं, अर्थात् आत्मतत्त्व जिस प्रकार हमारे अंदर रहता है उसी प्रकार इन सबके अन्दर भी उपस्थित है, उनके प्रति सचेतन है, इनकी गति को संचालित करता है, जिन चीजों का रूप वह ग्रहण करता है, जिस प्रकार उनमें निवास करने में आनंदमय रहता है उसी प्रकार उन्हें अपने अन्दर समाये रहने में भी आनन्दमय बना रहता है। जैसे आकाश घट को अपने अन्दर धारण करता है और साथ ही मानो उसमें समाया भी रहता है, वैसे ही यह आत्मतत्त्व या ब्रह्म सब भूतों को धारण करता है और साथ ही उनमें व्याप्त भी रहता है, किसी भौतिक अर्थ में नहीं, वरन् आध्यात्मिक अर्थ में; और यही उनकी यथार्थ सत्ता है। आत्मा के इस अन्तर्व्यापी स्वरूप का हमें साक्षात्कार करना होगा; सब भूतों में अवस्थित इस आत्मा के हमें दर्शन करने होंगे और अपनी चेतना में हमें यही बन जाना होगा... इस आत्मा को, जो हमारा निज स्वरूप है, अन्ततः हमारी आत्म-चेतना के लिए इस रूप में प्रकट करना होगा कि यह इन सब भूतों को अतिक्रम करता हुआ भी इन सब के साथ पूर्णतया एक है। हमें इसे केवल एक ऐसे आत्मा के रूप में नहीं देखना होगा जो सबको धारण करता है तथा सब में व्याप्त है, वरन् ऐसे आत्मा के रूप में भी जो सब कुछ है, जो अंतर्यामी आत्मा ही नहीं है, अपितु नाम और रूप भी है, गति और गति का स्वामी है तथा मन, प्राण और शरीर भी है।
इस प्रकार ये तीन अनुभूतियाँ हैं। एक है कि परमात्मा सभी कुछ को धारण करते हैं, दूसरी है कि सभी कुछ में परमात्मा व्याप्त हैं और तीसरी सबसे महत्त्वपूर्ण अनुभूति है कि सभी कुछ परमात्मा ही हैं।
यदि यह अनुभूति एकांगी हुई तो हमें 'सर्वेश्वरवादी' एकात्मकता का साक्षात्कार होता है, उन 'एकमेव' का जो सब कुछ हैं: पर यह सर्वेश्वरवादी दर्शन केवल आंशिक दर्शन ही है। यह सारा संसार-विस्तार ही आत्मा का संपूर्ण स्वरूप नहीं है, एक 'शाश्वत' है जो इससे महत्तर है केवल जिसके द्वारा ही इस संसार-विस्तार का अस्तित्व संभव है। ब्रह्माण्ड भी अपने सम्पूर्ण तत्त्वों से संपन्न भगवान् नहीं है, अपितु यह उनकी केवल एक आत्माभिव्यक्ति है, उनकी आत्मसत्ता की एक सच्ची पर गौण क्रिया है। ये सारे आध्यात्मिक अनुभव पहली दृष्टि में चाहे कितने ही परस्पर भिन्न या विरुद्ध हों, फिर भी इनका सामंजस्य हो सकता है यदि हम एकांगी रूप से किसी एक या दूसरे पर ही बल देना बंद कर दें और यदि इस सीधे-सादे सत्य को समझ लें कि भगवत्तत्व वैश्विक अस्तित्व से कोई महत्तर वस्तु है, परन्तु फिर भी सारा विश्व और विश्व के सारे भिन्न-भिन्न पदार्थ वही भगवान् हैं, और कुछ नहीं- हम कह सकते हैं कि वे भगवान् के ही द्योतक हैं। अवश्य ही ये रूप किसी अंश में या अपने समुच्चय में पूरी तरह से 'वह' नहीं हैं परंतु फिर भी यदि ये भगवत्सत्ता की ही कोई चीज न होते, और उससे भिन्न कोई दूसरी ही चीज होते तो ये भगवान् के सूचक नहीं हो सकते थे। 'वह' ही सत्-तत्त्व है; परंतु ये रूप उन्हीं की अभिव्यंजक यथार्थताएँ ' हैं। वासुदेवः सर्वमिति से यही अभिप्रेत है; भगवान् यह सारा जगत् जो कुछ है वह सब हैं, जो कुछ इस जगत् में है वह सब हैं और इस जगत् से अधिक जो कुछ भी है वह भी वही हैं।
------------------------
* भले ही हमारे मन में ये हमें निरपेक्ष सत्य के सामने अपेक्षाकृत असत् ही प्रतीत होते हों। शंकराचार्य का मायावाद, उसके तार्किक आधार को अलग करके, उसे आध्यात्मिक अनुभूति की दृष्टि से देखा जाए तो इसी सापेक्ष (relative) असत् का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनमात्र प्रतीत होता है। मन-बुद्धि के परे यह समस्या लुप्त हो जाती है क्योंकि वहाँ ऐसी कोई समस्या कभी थी ही नहीं। धार्मिक संप्रदायों तथा दर्शन अथवा योग पद्धतियों के परस्पर भेदों के पीछे निहित भिन्न-भिन्न अनुभवों का जब रूपांतरण कर दिया जाए तो वे अपने भिन्न-भिन्न मानसिक क्रमों को छोड़ देते हैं और जब उन्हें अपनी उच्चतम समान प्रगाढ़ता या तीव्रता तक उठा लिए जाए तो आपस में समन्वित हो जाते हैं और अतिमानसिक अनन्तता में एकीभूत हो जाते हैं।
इन तीनों अनुभवों को यदि हम संकुचित दृष्टिकोण से लें तो हम भगवान् को इन तीन सूत्रों में बाँध देंगे और इन तीन को ही भगवान् का संपूर्ण स्वरूप घोषित कर देंगे। हमारे वैदिक ऋषियों को इस बात का बोध था कि परमात्मा को किन्हीं भी अनुभवों में, किन्हीं भी सूत्रों में नहीं बाँधा जा सकता। और परमात्मा की अभिव्यक्ति भी उनके सत्स्वरूप का एक अतिक्षुद्र अंश मात्र ही है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वे इस अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं हैं। परन्तु उनका सत्स्वरूप अभिव्यक्ति से सीमित नहीं है, वह तो उसके परे भी है। इसीलिये हमारे शास्त्रों में परात्पर की परिकल्पना है क्योंकि परमात्मा सभी कुछ को सर्वथा अतिक्रम कर जाते हैं, वे सभी सूत्रों से परे हैं। इसलिए परमात्मा केवल इस दृष्टिकोण से ही परमात्मा नहीं हैं कि जो कुछ अभिव्यक्त हुआ है वह वे ही हैं, अपितु वे इस दृष्टिकोण से परमात्मा हैं कि उनके सिवा कुछ और है ही नहीं, वे ही सब कुछ हैं। अतः सब कुछ है तो उन्हीं का रूप परन्तु वे उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ हैं। उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि उनका स्वरूप तो अगम, अचिंत्य, वर्णनातीत है। इसीलिये जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ हमारी कल्पना में है, जो कुछ हमारे अनुभव में है वह सब भी और जो कुछ नहीं है वह सब भी और उससे परे भी जो कुछ है वह सब कुछ परमात्मा ही है। अन्य किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, 'वासुदेवः सर्वमिति', और चूँकि विरला ही कोई इस बात को जान सकता है इसीलिए यह दुर्लभ है।
परंतु सामान्यतया चेतना इतनी संकुचित होती है कि किसी छोटे-मोटे अनुभव को ही व्यक्ति सब कुछ बताकर उसकी नुमाइश करने लगता है। अब चूंकि मनुष्य का मन संकुचित है इसलिए उसके द्वारा भगवान् का जो कोई अनुभव प्राप्त होता है वह संकुचित ही होता है। हालाँकि मानसिक चेतना में किये अनुभव अपने आप में सारे सही हैं परंतु उनका किसी का भी परमात्मा के स्वरूप पर एकाधिकार नहीं है। वैसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश अनेक दर्पणों में पड़ता है और सभी में उसी एक सूर्य का प्रतिबिंब होने पर भी वह किसी में भी बँध नहीं जाता। वैसे ही मानसिक चेतना में उस सत्य के जितने भी बिंब बनते हैं वे हैं तो उस सत्य के ही बिंब परंतु उनका उस सत्य पर एकाधिकार नहीं होता और न ही वह पूर्ण सत्य उनमें समाहित होता है। वह तो उन सब से परे होता है। अतिमानसिक चेतना में ही पूर्ण सत्य के दर्शन हो सकते हैं। भगवान् इतने असीम हैं कि वे हमारी असीम-संबंधी धारणा से भी सीमित नहीं होते। वे वास्तव में ही सभी चीजों को, हमारे ऊँचे से ऊँचे मानसिक विचारों, मानसिक सूत्रों को अतिक्रम कर जाते हैं। इसीलिए गीता भगवान् को अनेक स्थानों पर अप्रमेय पद से संबोधित करती है। श्रीअरविन्द भी इस पद की बड़ी प्रशंसा करते हैं और अपनी टीका में भगवान् के लिए इस पद का प्रयोग करते हैं।
गीता में भगवान् का संबोधन करने के चार शब्द हैं - परमात्मा, परमेश्वर, परमब्रह्म और पुरुषोत्तम। यदि हम पुरुष आदि के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वे पुरुषोत्तम हैं। यदि हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो वे हमारी वैयक्तिक और वैश्विक आत्मा से परे परमात्मा हैं। यदि सारी सृष्टि के नियंता तथा इसके ईश्वर के रूप में देखें तो वे इस सबके परे परमेश्वर हैं। और यदि इस सारी अभिव्यक्ति का निषेध कर हम एक ऐसी सत्ता की बात करें जो इनके परे है तो वह ब्रह्म है। और उसके भी परे परमब्रह्म है। ये सभी पद एक ही परम सत्ता को द्योतित करते हैं पर वर्णन में जब हम भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से बात करते हैं तब भिन्न पदों का प्रयोग करते हैं। और इससे हमारी भारतीय संस्कृति की समृद्धता का भान होता है कि कितने विविध रूपों में यहाँ महापुरुषों को भगवान् का साक्षात्कार हुआ है अन्यथा अन्य संस्कृतियों में तो किसी एक ही नाम से उस परम सत्ता को संबोधित कर दिया जाता है, जबकि भारतीय संस्कृति में तो परमात्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों के भी भिन्न-भिन्न नाम हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल भिन्न नाम ही हैं, इनकी क्रियाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं।
कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।। २० ।।
२०. भिन्न-भिन्न प्रकार की बाह्य कामनाओं के वशीभूत होकर, जिससे उनका ज्ञान अपहृत हो जाता है, मनुष्य अपनी स्वयं की प्रकृति द्वारा प्रेरित होकर इस या उस विधि-नियम को स्थापित कर अन्य देवताओं का आश्रय ग्रहण करते हैं।
.....जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ भक्त भगवान् को उनके समग्र सर्वसमावेशी सत्य (वासुदेवः सर्वमिति) को जानकर उनकी ओर नहीं जाता, अपितु भगवान् के ऐसे अधूरे नाम और रूप गढ़ता है जो स्वयं उसकी अपनी ही आवश्यकता, मनोदशा और प्रकृति के प्रतिबिंब मात्र होते हैं और इन बिंबों को वह अपनी स्वाभाविक या प्राकृत लालसाओं में सहायता पहुँचाने या उन्हें तुष्ट करने के लिए पूजता है।... अब यह प्रश्न किया जा सकता है वह भक्ति उदार कैसे हो सकती है जो भगवान् को, वे जो सांसारिक वरदान दे सकते हैं केवल उन्हीं को पाने के लिए ढूँढ़ती है या फिर उन्हें दुःख कष्ट में एक आश्रय के रूप में खोजती है और स्वयं भगवान् के लिए ही भगवान् को नहीं चाहती? क्या ऐसी भक्ति में अहंकारिता, दुर्बलता और वासना-कामना ही प्रधान नहीं रहती, इसलिए क्या इसे भी निम्न प्रकृति की ही चीज नहीं समझना चाहिए?
निःसन्देह, समस्त आराधन-रूप प्रेम के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति होती है और यहाँ तक कि जब यह अज्ञानपूर्वक तथा किसी सीमित पदार्थ को अर्पित किया जाता है तब भी विधि-विधान के अभाव तथा उसके परिणामों की तुच्छता में से भी आध्यात्मिक वैभव की कुछ छटा दिखायी देती है। क्योंकि प्रेम जो कि पूजा है, एक साथ ही अभीप्सा भी होता है और एक तैयारी भी : यह अपनी अविद्यागत क्षुद्र सीमाओं के भीतर भी एक आश्चर्यजनक साक्षात्कार की झलक प्राप्त करा सकता है जो भले अभी न्यूनाधिक अंघ तथा आंशिक हो; क्योंकि ऐसे क्षण आते हैं जब हम नहीं अपितु एकमेव हो प्रेम करने वाला व हममें प्रेम का पात्र होता है और एक मानवीय भावावेश भी इस अनंत प्रेम और प्रेमी की जरा-सी झाँकी से उदात्त एवं महिमान्वित हो सकता है। यही कारण है कि देवता एवं प्रतिमा की अथवा किसी आकर्षक व्यक्ति या श्रेष्ठ पुरुष की पूजा को तुच्छता की दृष्टि से नहीं देखना चाहियेः क्योंकि ऐसी पूजाएँ ऐसे सोपान होती हैं जिनके द्वारा मानवजाति अनंत के उस आनंदपूर्ण भावावेश और परमानंद की ओर गति करती है जो कि अनंत को सीमित करते हुए भी उसको हमारी अपूर्ण दृष्टि के समक्ष प्रकाशित करती हैं, जब कि अभी हमें उन निम्न सोपानों को, जो प्रकृति ने हमारी प्रगति के लिये बनाये हैं, प्रयोग में लाना तथा अपनी उन्नति के क्रमों को अंगीकार करना होता है। हमारी भावात्मक सत्ता के विकास के लिये कई प्रकार की प्रतिमा-पूजाएँ अनिवार्य हैं, और वह जो ज्ञानी है तब तक किसी भी अवसर पर प्रतिमा को भंग करने के लिये उतावला न होगा जब तक कि वह इसके स्थान पर उस सद्वस्तु को, जिसका कि यह प्रतीक मात्र है, उपासक के हृदय में प्रतिष्ठित न कर सके।
यहाँ प्रतिमा से अर्थ केवल किसी मन्दिर में पूजी जाने वाली प्रतिमा से नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में किसी मानसिक आदर्श को या किसी विचार को लेकर चलता है और उसके प्रति निष्ठा रखता है। अन्य कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा लेकर चलता है। अपने-अपने गठन के अनुसार हर एक को अपने-अपने इन आदर्शों, विचारों, अभीप्साओं आदि में कोई सत्य दिखाई देता है और चूंकि उसके लिए वह सत्य होता है इसलिए उसके लिए वह एक प्रतिमा बन जाती है और उसके लिए परमात्मा की अभिव्यक्ति उस रूप में होती है। अपने आप में तो भगवान् हमारी किन्हीं भी ऊँची से ऊँची धारणाओं से, परिकल्पनाओं से बिल्कुल परे हैं और इनमें से किन्हीं में भी पकड़ में नहीं आते परंतु जिसका जिस प्रकार का गठन होता है उसकी चेतना के लिए उस सत्य की अभिव्यक्ति उसी प्रतिमा के रूप में हो जाती है। अब चूंकि पशु चेतना के लिए मनुष्य उनकी चेतना को सर्वथा अतिक्रम कर जाते हैं इसलिए उन्हें वे ही देवता सदृश दिखाई देते हैं। उसी प्रकार मानव चेतना में भी ज्यों-ज्यों विकास होता है देवत्व की उसकी परिकल्पना भी विकसित होती जाती है।
अब प्रतिमा बनाने के पीछे क्या औचित्य है? यदि मनुष्य को अपने क्षुद्र अहं से निकलकर किसी अन्य पूजा के पात्र का सहारा न हो तो वह कभी भी एकाएक सच्चे प्रेम तक, दिव्य प्रेम तक पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए जिस भी तरीके से मनुष्य अपने आप को भूलकर किसी अन्य विषय पर केंद्रित होता है, उसके प्रति अपने को समर्पित करता है, उतना ही उसे अपने अहं से कुछ छुटकारा मिलता है और वह आगे प्रगति करता है। यह प्रतिमा परिवार, समाज या राष्ट्र के रूप में हो सकती है, किसी आदर्श, विचार या सिद्धांत के रूप में हो सकती है, किसी व्यक्ति, प्रेरक भाव या अभीप्सा के रूप में हो सकती है। इनके सहारे व्यक्ति विकसित होता जाता है और अपने आप को किसी के प्रति समर्पित करने की क्षमता भी उसमें विकसित होती जाती है। अब यद्यपि इन सभी प्रकार के प्रेमों के पीछे मूल में भगवान् का प्रेम ही होता है तो भी प्रत्यक्ष रूप से उसकी (भागवत् प्रेम की) अभिव्यक्ति सबसे क्षीण रूप से ही रही है। उसका कारण है कि हमने जिन भी प्रतिमाओं का निर्माण कर रखा है, प्रेम के जिन भी रूपों का वरण कर रखा है उनमें हमारा प्रेम निःस्वार्थ नहीं है अपितु उसमें हम अपना प्राणिक या मानसिक या अन्य कोई सुख, अन्य कोई तुष्टि ढूँढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अपने देश के प्रति समर्पित व्यक्ति को यह भाव रहता है कि उसका देश सबसे महान् हो। यदि कोई किसी विचार के प्रति समर्पित है तो यह प्रयास रहता है कि वह विचार चरितार्थ हो जाए तो उसे कितना सुख मिलेगा। इस प्रकार इन सभी प्रकार के उद्देश्यों में कहीं न कहीं रहती तो अहं की ही तुष्टि है भले वह कहीं सूक्ष्म रूप से हो तो कहीं अधिक प्रत्यक्ष रूप से। केवल दिव्य प्रेम अहैतुक होता है। परंतु आरंभ में ही व्यक्ति इस अवस्था तक नहीं पहुँच सकता इसलिए वह विभिन्न प्रतिमाओं की सहायता से धीरे-धीरे विकसित होता है। हमारी पाशविक प्रवृत्ति हम पर इतनी हावी होती है कि जब तक हमें बदले में कुछ प्राप्त न हो तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। भारतीय संस्कृति में सदा ही इस बात का भान होने के कारण कभी भी किसी के प्रति समर्पण के भाव को गौण नहीं समझा गया और उस भाव को हतोत्साहित करने की बजाय सदा ही उसे बढ़ावा दिया गया। इसीलिए यहाँ हम मित्र के प्रति मित्र के प्रेम और त्याग की, सगे-संबंधी के प्रति, माता-पिता के प्रति, देश के प्रति त्याग की कथाएँ सुनते हैं और उन्हें बहुत ही सराहा जाता रहा है। इसीलिए गीता भी मानती है कि भले आर्त्त हो, अर्थार्थी हो या जिज्ञासु हो, भगवान् की ओर चलने वाले सभी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में सदा ही यह बोध रहा है कि पूजा का पात्र भले ही कितना भी तुच्छ क्यों न हो, जब तक कि व्यक्ति को किसी श्रेष्ठतर उद्देश्य के लिए, पूजा के किसी महत्तर पात्र या प्रतिमा के लिए तैयार न कर दिया जाए तब तक उसकी पूर्व की प्रतिमा को भंग नहीं करना चाहिये अन्यथा तो उसे अपनी अहं की सीमाओं से बाहर निकलने का कोई आधार ही नहीं रहेगा। जो भी प्रेम के रास्ते पर, आत्मसमर्पण के रास्ते पर चल रहा है, चाहे वह रास्ता कितना भी क्षुद्र क्यों न हो, चाहे उसके पीछे कितना भी हिसाब-किताब अथवा माँग क्यों न हो, वे सभी अच्छे हैं। इसीलिये गीता कहती है 'उदाराः सर्व एवैते।'
प्रश्न : क्या इसमें ये दो चीजें हो सकती हैं जिसमें एक में तो व्यक्ति को अपने आदर्श के अलावा या जिस किसी प्रतिमा को उसने पकड़ रखा है उसके अलावा और कुछ पता नहीं होता और उसके लिये वही सब कुछ होती है, और दूसरी में वह किसी प्रतिमा को अपनाता अवश्य है परंतु उसे भान होता है कि वह प्रतिमा किसी परम तत्त्व की प्रतिनिधि मात्र है और वह उसे यथासमय छोड़ सकता है?
उत्तर : नहीं ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में कभी भी प्रतिनिधि को गौण नहीं मानते। सदा ही उसे तो परम ही मानते हैं तभी तो हम कहते हैं कि 'गुरु साक्षात् परम् ब्रह्म'। वे तो उसे साक्षात् परंब्रह्म ही मानते हैं न कि परम का कोई प्रतिनिधि। अब क्या हम श्रीमाताजी व श्रीअरविन्द को परम् का प्रतिनिधि मानेंगे? हमारे लिए तो वे ही परम् हैं। यों तो सभी कुछ परम् है, परंतु किसी एक अर्थ में लेने पर इस बात की अधिकांश शक्ति चली जाती है। उदाहरण के लिए हमारे भिन्न-भिन्न पुराणों में भिन्न-भिन्न देवताओं को परम् भगवान् के रूप में प्रतिपादित किया गया है जिसमें अन्य देवों को उनसे कनिष्ठतर बताया गया है। शिव पुराण में भगवान् शिव को परम देव बताया गया है, गणेश पुराण में गणेश को परम् बताया गया है, वहीं देवी पुराण में देवी को ही परम् बताया गया है। यह एक ऐसा सत्य है जो हमारी संस्कृति में अंतर्बोधात्मक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण सर्वमान्य रहा है और किसी को इससे कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। परंतु मानसिक रूप से इसे नहीं समझा जा सकता कि परम् तो कोई एक ही हो सकता है, सारे ही परम् कैसे हो सकते हैं। और इसी कारण बहुत से मानसिक दृष्टिकोणों में हम इसके विरुद्ध आक्षेप पाते हैं। परंतु यदि हम अपने आराध्य देव को वास्तव में ही परम् न मानें तो उनकी आराधना से हमें क्या लाभ होने वाला है। कभी हम किसी गुरुवादी को यह कहते नहीं सुनते कि सभी परम् हैं इसलिए वह अपनी सुविधानुसार गुरु की आज्ञापालन और सेवा के लिए स्वतंत्र है और यहाँ तक कि गुरु बदलने के लिए भी स्वतंत्र है। सभी सच्चे शिष्य गुरु को ही एकनिष्ठ रूप से परम मानते हैं और अपना संपूर्ण जीवन निर्विवाद रूप से उनके चरणों में अर्पित करते हैं। शिष्य के लिए गुरुवाक्य ही अंतिम होता है। इसीलिये कहते हैं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं। यह केवल कोई मानसिक दृष्टिकोण नहीं है अपितु एक गंभीर आध्यात्मिक सत्य है। और इस एकनिष्ठता के प्रभाव से जब व्यक्ति की आँखें खुलती हैं तब उसे सर्वत्र अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। गीता भी इस स्थिति का वर्णन करती हुई कहती है, "जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर समस्त भूतों में मुझसे प्रेम करता है वह योगी चाहे जिस प्रकार रहे और कर्म करे मुझ में ही रहता और कर्म करता है।" जैसे श्रीरामकृष्ण परमहंस को तो सभी जगह माँ काली का ही दर्शन होता था। परंतु इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि व्यक्ति को जब सर्वत्र अपने गुरु का ही रूप नजर आए तो वह अपने गुरु को छोड़ कर कहीं भी जा सकता हो। सच्चा साधक सदा ही नैष्ठिक भाव रखता है न कि किसी प्रकार का कोई अधकचरा मानसिक दृष्टिकोण कि जब सभी ब्रह्म है तो वह तो किसी के पास भी जा सकता है। गुरु के प्रति निष्ठा का भाव तो एक सर्वथा भिन्न भाव है जिसे सतह पर नहीं समझा जा सकता।
प्रश्न : इसका क्या अर्थ है, "न ही वह जो ज्ञानी है तब तक किसी भी अवसर पर प्रतिमा को भंग करने के लिये उतावला होगा जब तक कि वह इसके स्थान पर उस सद्वस्तु को, जिसका कि यह प्रतीक मात्र है, उपासक के हृदय में प्रतिष्ठित न कर सके"?
उत्तर : इसका यह अर्थ है कि प्रतिमा के माध्यम से सत्य का जितना तत्त्व अभिव्यक्त हो रहा है उससे अधिक गहराई तक यदि व्यक्ति को न ले जाया जाए तब तक वह उस प्रतिमा को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि भले वह प्रतिमा कितनी भी सीमित क्यों न हो परंतु उस व्यक्ति को तो अपना सब कुछ उसी के माध्यम से मिलता है। इसलिए जब तक उसे उससे गहनतर सत्य के दर्शन न कराए जाएँ तब तक वह उस प्रतिमा को नहीं छोड़ सकता और छोड़ना चाहिये भी नहीं अन्यथा तो उसके पास अपने अहं से दूर हट कर ऊपर आरोहण करने का कोई आधार ही नहीं बचेगा। वास्तव में सब कुछ भगवान् का अधिकाधिक आत्म-उन्मीलन है। चेतना के एक अधिक गहरे स्तर पर हमें परमात्मा के अधिक प्रगाढ़ दर्शन प्राप्त होते हैं। और ज्यों-ज्यों हम उस सद्वस्तु के अधिकाधिक निकट जाते हैं त्यों-त्यों हमें उसकी और अधिक अंतरंग अनुभूति, अधिक प्रगाढ़ स्पर्श प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि व्यक्ति यह सोचे कि अपने गुरु या इष्ट देव की सहायता से और उन्हें अतिक्रम करके वह भगवान् के पास चला जाएगा। वह उस परम सद्वस्तु, परम तत्त्व को उसके माध्यम से नहीं अपितु स्वयं उसी के अंदर देखेगा। अब इसको समझने के लिए, यदि कोई श्रीकृष्ण से प्रेम करता है तो एक भाव तो यह है कि वह उनके शरीर से या बाहरी रूप से ही प्रेम करता हो, वहीं दूसरा भाव वह है जो उनके शरीर के अतिरिक्त उनके अंतर्तत्त्व को भी जानता हो। वह उनसे और भी प्रगाढ़ रूप से प्रेम कर सकता है। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों साधक उनकी अधिकाधिक गहराई में, उनके सत्स्वरूप में प्रवेश करता जाता है त्यों ही त्यों उसका प्रेम अधिकाधिक गहरा होता जाता है। परंतु इसका यह गलत अर्थ लगाना हुआ कि व्यक्ति श्रीकृष्ण को छोड़कर भगवान् शिव के पास चला जाए क्योंकि वे परात्पर देव हैं। यह एक सूक्ष्म भेद है। इसलिए व्यक्ति जब सद्वस्तु की अधिकाधिक गहराई में जाने लगता है तब वह उसके बाहरी रूप को ही नहीं अपितु उसके गहरे अंतरंग स्वरूप को भी देखता है और ज्यों-ज्यों वह उसके अधिकाधिक अंतरंग स्वरूप को देखता है वह उससे उतने ही अधिक प्रगाढ़ रूप से प्रेम करने लगता है। इसी भाव के कारण जहाँ किसी के लिए वह प्रतिमा, वह विग्रह कोरी प्रतिमा मात्र ही रहेगी वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए वह साक्षात् परमात्मा का श्रीविग्रह होगी। इसलिए श्रीअरविन्द कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने जो भी रूप अभिव्यक्त किये हैं अपने सत्स्वरूप में वे उनसे कहीं महत्तर हैं। जिस रूप में वे प्रकट हुए और लीला आदि कीं वे तो उनके बाहरी रूप और क्रियाकलाप हैं। उनका पूर्ण स्वरूप इन सबसे अनंततः विशाल है। इसलिए हमें उन्हें केवल इन्हीं रूपों से नहीं बाँधना चाहिये।
पर यदि किसी व्यक्ति को श्रीकृष्ण की लीला और रास में ही आनन्द आ रहा हो तो जब तक उस व्यक्ति को उससे भी अधिक गहराई में नहीं ले जाया जा सके और भगवान् के अधिकाधिक अंतरंग आयामों का दर्शन न कराया जा सके तब तक उसके वर्तमान भाव को भंग नहीं करना चाहिये। आखिर रास आदि भी तो भगवान् श्रीकृष्ण की अभिव्यक्ति मात्र ही तो हैं। इन सब अभिव्यक्तियों से वे सीमित नहीं हो जाते। उनका निजस्वरूप इन सब अभिव्यक्तियों से कहीं अधिक विशाल है। इसीलिए तो कहते हैं कि हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। पर यदि कोई शबरी के प्रसंग से ही द्रवित हो उठता है और उसमें ही उसे आनंद आता है तो उसके लिए तो वही ठीक है। पर यदि श्रीराम के स्वरूप में और अधिक गहरे रूप से पैठा जा सके तो अधिक श्रेष्ठ है। वास्तव में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि परमात्मा का रूप नहीं है। बात केवल इतनी है कि उस रूप की कितनी गहराइयों तक हम जा सकते हैं। स्वयं श्रीअरविन्द को करनाली स्थित दुर्गा मंदिर में जगदम्बा के दर्शन प्राप्त हुए। अब जो बाहरी पूजा-पाठ करते हैं उन्हें वह केवल एक प्रतिमा दिखाई देती है जबकि श्रीअरविन्द के लिए तो वे साक्षात् जगदम्बा के रूप में प्रकट हो गईं। आंतरिक दृष्टिकोण में कोई मानसिक रूढ़िवाद नहीं रहता। इसीलिए इस संदर्भ में श्रीकृष्णप्रेम कहते थे, "मैं किसी अपराध क्षमा-याचना के प्रकार की अनमनी-सी पूजा की बात नहीं करता जो कि प्रतिमा को एक प्रतीक या फिर ध्यान लगाने के किसी केंद्र के रूप में काम में लेती है, अपितु उस सच्ची पूर्णरूपेण सेवा की बात कर रहा हूँ जो विग्रह को स्वयं कृष्ण के रूप में देखती है।" (योगी श्रीकृष्णप्रेम, पृष्ठ १६३)
अतः कहने का तात्पर्य है कि हम अपने पूजा के पात्र की ही अधिकाधिक गहराई में प्रवेश कर सकते हैं, यह नहीं कि हम उस पूजा के पात्र का ही त्याग कर दें और किसी अन्य का वरण कर लें।
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ।। २१ ।।
२१. जो कोई भक्त मेरे जिस किसी रूप की श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहता है, उस भक्त की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ और अचल बना देता हूँ।
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ।। २२॥
२२. वह भक्त, उस श्रद्धा से युक्त होकर उस रूप की आराधना करता है और उसके द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है; निःसंदेह मैं स्वयं ही हूँ जो उसे ये सब चीजें प्रदान करता हूँ।
यदि मनुष्य को उसके जिस भी किसी वर्तमान स्तर से भगवान् की ओर जाने की अनुमति न होती और केवल वे ही भगवान् के पास जा सकते थे जिनमें सच्ची भक्ति आदि होती, तब तो भगवान् की ओर कदाचित् ही कोई मुड़ सकता था। परंतु भगवान् कहते हैं कि जिस किसी रूप से भी कोई उनकी ओर चलता है उसकी उस श्रद्धा को वे दृढ़ बना देते हैं। आरंभ में व्यक्ति घोर तामसिक तथा राजसिक अवस्था में होता है। ऐसे में वह केवल तामसिक और राजसिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनकी ओर मुड़ता है। आरंभ में उसे कोई भौतिक लाभ की अपेक्षा होती है, किसी प्राणिक सुख की या लाभ की अपेक्षा होती है। मंदिर आदि में लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाता है। बहुत तो ऐसे हैं जो इस भय से जाते हैं कि ऐसा न करना उन्हें संकट में डाल सकता है। इसलिए यदि इन सभी चीजों को अनुमति न दी जाती तो शायद ही कभी कोई भगवान् की ओर चल सकता था। और जब व्यक्ति धीरे-धीरे घोर भौतिक और प्राणिक चेतना से कुछ अधिक विकसित होता है तब उसे महसूस होने लगता है कि केवल किन्हीं निम्न हेतुओं के लिए भगवान् की ओर चलना कोई श्रेष्ठ भाव नहीं है। और इस प्रकार धीरे-धीरे उसका भाव उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है और फिर केवल किन्हीं हेतुओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि उसे भगवान् के निजस्वरूप में रस आने लगता है। क्योंकि सबसे महत्त्वपूर्ण चीज है किसी प्रकार भी भगवान् के संपर्क में आ जाना और इसीलिए व्यक्ति की श्रद्धा का विषय कितना भी छोटा क्यों न हो पर उसे प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। जिन लोगों की शालिग्राम में आस्था है उन्हें उनके द्वारा उत्तर मिलता है, जिनकी किसी तीर्थ में आस्था है उन्हें वहाँ संपर्क प्राप्त होता है। इसलिए जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है भगवान् उसकी उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं।
....परम् देव इन सब भक्तों को उनकी अपूर्ण दृष्टि होने के कारण उन्हें अस्वीकार नहीं कर देते। क्योंकि भगवान् अपनी परम् परात्पर सत्ता में अजन्मा, अव्यय और इन सब आंशिक अभिव्यक्तियों से श्रेष्ठ होने के कारण सहज ही किसी प्राणी की समझ में नहीं आ सकते। वे माया, अपनी योगमाया, के इस अतिविशाल आवरण में अपने-आप को ढके हुए हैं जिसके द्वारा वे जगत् के साथ एक हैं और फिर भी उसके परे हैं, अंतर्यामी हैं, पर छिपे हुए हैं, सभी हृदयों में अवस्थित हैं, पर हर किसी के लिए प्रकट नहीं हैं। प्रकृतिस्थ मनुष्य समझता है कि प्रकृतिगत सभी अभिव्यक्तियाँ अथवा सभी पदार्थ भगवान् ही हैं जब कि यथार्थ में ये सब केवल उनके कार्य, शक्तियाँ और आवरण मात्र हैं। भगवान् समस्त भूत, वर्तमान और भविष्य के जन्मों को जानते हैं पर उन्हें कोई नहीं जानता। इस कारण यदि प्रकृति में अपनी क्रिया के द्वारा सब प्राणियों को इस प्रकार भरमाकर वे इन सब पदार्थों के अन्दर उन्हें दर्शन न दें तो माया में बद्ध किसी मनुष्य या जीव के लिए कोई दिव्य आशा न रह जाएगी। इसलिए इन भक्तों की प्रकृति के अनुसार, जैसे भी ये भगवान् की ओर चलते हैं उसी रूप में भगवान् इनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और बदले में दिव्य प्रेम और करुणा द्वारा उनका उत्तर देते हैं। आखिर ये रूप हैं भी तो उन्हीं का एक ऐसा आविर्भाव जिसमें से होकर अपूर्ण मानवी बुद्धि उनका स्पर्श पा सकती है, ये कामनाएँ ही वह प्रथम साधन' बन जाती हैं जिससे हमारे हृदय उनकी ओर मुड़ते हैं: और, न ही किसी भी प्रकार की भक्ति निरर्थक या निष्प्रभावी होती है, भले उसकी कैसी भी सीमाएँ या कमियाँ क्यों न हों।
------------------------
'भगवान् से अपना समस्त कल्याण चाहते चाहते वह अंत में भगवान् में ही अपना समस्त कल्याण खोजने लगेगा। अपने सब सुखों के लिए भगवान् पर निर्भर रहने के द्वारा वह भगवान् में ही अपने सभी सुखों को स्थापित करना सीख लेगा। भगवान् को उनके रूपों और गुणों में जानकर वह उन्हें उस समग्र और परात्पर रूप में जानने लगेगा जो सब पदार्थों का मूल है।
....कितने ही लोग हैं जिनमें धार्मिक श्रद्धा है और धार्मिक भाव है और जो कि जब वे पूर्ण रूप से यह धारणा रखते हैं कि उनके भगवान् उन्हें आगे ले जा रहे हैं तब भी, वस्तुतः अपने हृदय के आवेगों, अपनी कामना की तृष्णाओं, अपनी इंद्रियों की आतुरताओं और अपने ही विचारों के आदेशों का ही अनुसरण कर रहे होते हैं! और वे सफल रहते हैं, क्योंकि भगवान् उनका मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। उनके लिए यह मार्ग 'उन्होंने' ही चुना है, और क्योंकि 'उन्होंने' इसे चुना है इसलिए यह उनके लिए सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और सर्वाधिक फलप्रद मार्ग है। फिर भी यह उनका अपना भगवान् होता है - जैसे नास्तिक मानते हैं उस रूप में नहीं कि उस भगवान् को उन लोगों ने अपने स्वरूप के अनुसार गढ़ लिया है, परंतु इस रूप में कि ये ऐसे भगवान् हैं जो स्वयं को उस रूप में बना लेते हैं जिस रूप में वे लोग पसंद करते हैं, उस रूप में जो उनकी प्रकृति या उनके विकास के सर्वाधिक उपयुक्त हो। "जिस भी तरीके से मनुष्य मेरे पास आते हैं, उसी रूप iv.11 में मैं उनसे प्रेम करता हूँ और उनका आलिंगन करता हूँ।" यह एक अगाध गहराई की बात है जिसमें भगवान् और धर्म के सत्य का संपूर्ण बीज या मर्म निहित है। आखिरकार, केवल इसी तरीके से सीमित का परम् से मिलाप हो सकता है, जिसकी अपनी एक प्रकृति या धर्म है उस जीव का उससे मिलन हो सकता है जो प्रकृति या धर्म की सभी सीमाओं से परे है... फिर भी, जो मार्ग (निम्नतर) देवों के प्रति हमारी अधीनता के द्वारा हमें आगे ले जाता है उसकी अपेक्षा भगवान् से मिलने का एक उच्चतर मार्ग भी है।
हमारी सारी इच्छाएँ, कामनाएँ, कर्म-अकर्म आदि सभी कुछ रास्ते की घटनाओं के रूप में हैं। और जब ये चीजें घट चुकी होती हैं तब इनके प्रति यह मनोभाव हो कि भगवान् की ही इच्छा से जो अच्छा से अच्छा संभव था वही घटित हुआ है। परंतु यह तर्क उस घटना के घटित होने से पूर्व नहीं दिया जा सकता। सिद्धांततः तो भगवान् की इच्छा के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता परंतु जब व्यक्ति के पास चुनाव का समय हो उस समय व्यक्ति जो चयन करता है वह बहुत महत्त्व रखता है। क्योंकि यह चयन भगवान् के विधान में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण यंत्र है जिसके द्वारा वे दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए व्यक्ति कोई उदासीन मनोभाव नहीं अपना सकता। उसे तो जो कार्यक्षेत्र मिला है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना होता है। उसमें प्रमाद करके इस विचार का दुरुपयोग करना कि सभी कुछ भगवान् की ही इच्छा से होता है और इसलिए व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक मिथ्या और तामसिक विचार है। इसीलिए श्रीमाताजी कहती हैं कि सदा अपनी चेतना के शिखर पर बने रहो और तब सदा तुम्हारे साथ सर्वश्रेष्ठ ही होगा। परंतु यदि यह आदर्श स्थिति सदा ही न बनाई रखी जा सके तो भी किन्हीं संकटकालों या निर्णायक क्षणों पर तो व्यक्ति अभीप्सा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, दिव्य संकल्प के प्रति समर्पण के द्वारा अपनी उच्चतम नियति का आह्वान कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिये कि वह मानसिक रचनाएँ बनाए बिना, किन्हीं पूर्वाग्रहों से प्रभावित हुए बिना व्यवहार करे, क्रिया करे। इसलिए इच्छाओं और कामनाओं के वशीभूत हो कर्म करने की प्रकृति के अंतर्गत जो प्रवृत्ति रहती है उसी प्रकृति के अंदर यह व्यवस्था भी निहित रहती है कि व्यक्ति उच्चतर क्रिया के लिए अभीप्सा रखे, उच्चतर विधानों का आह्वान करे, निम्नतर चीजों को अस्वीकार करे और उनसे ऊपर उठे। प्रमादवश यह कह देना कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है इसलिए हमें कुछ करने की या फिर चयन करने की आवश्यकता नहीं है, यह भगवान् के प्रति दुर्भावना है। भले ही सिद्धांततः यह बिल्कुल सही है कि सब कुछ भगवान् की ही इच्छा से हो रहा है और हमारा अब तक का जो भी विकास रहा है वह भी भगवान् की ही इच्छा से ही रहा है और हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहा है परंतु ऐसा हम जो चीजें घट चुकी हैं उन्हीं के लिए कह सकते हैं, घटने से पूर्व नहीं जहाँ कि हमें चुनना होता है और जो चरितार्थ होगा उसमें वह चुनाव महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। व्यक्ति के लिए सदा ही चयन की संभावना खुली रहती है और यह उसके चयन पर निर्भर करता है कि उस पर कौनसा विधान लागू होगा। व्यक्ति अपने चयन से एक उच्चतर विधान को भी सक्रिय कर सकता है और अपने चयन के कारण अपनी स्थिति से नीचे भी गिर सकता है।
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।। २३ ।।
२३. किंतु क्षुद्र बुद्धिवाले मनुष्यों द्वारा चाहे जाने वाले ये फल अस्थायी हैं; देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं किंतु मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं।
और इस तरह से जो कुछ भी आध्यात्मिक लाभ होता है वह देवताओं की ओर ले जानेवाला होता है; वे केवल क्षर प्रकृति के नानाविध रूपों में स्थित भगवान् को ही अनुभव कर पाते हैं जो कर्मफल देनेवाले होते हैं। परंतु जो प्रकृति से अतीत समग्र भगवान् को पूजते हैं वे यह सब भी ग्रहण करते और इसे दिव्य बना लेते हैं, देवताओं को उनके परम् स्वरूप तक, प्रकृति को उसके शिखर तक चढ़ा ले जाते हैं और उनके परे परमेश्वर तक जा पहुँचते हैं, परम् पुरुष भगवान् का साक्षात्कार करते और उन्हें प्राप्त होते हैं।
यह एक ऐसी उक्ति है जिसका बहुत बार गलत अर्थ लगाया जाता है। इसका सहारा लेकर कुछ लोग विष्णु या भगवान् श्री कृष्ण की अन्य सभी देवताओं से वरीयता दिखाने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं कि शिव या शक्ति या अन्य देवता तो भगवान् श्रीकृष्ण से निचले स्तर पर हैं और इसके प्रमाण के रूप में वे यह श्लोक उद्धृत करते हैं। परंतु जगह-जगह पर हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार गीता का गलत अर्थ लगाया जा सकता है। श्रीअरविन्द के आलोक में यह एक बिल्कुल ही भिन्न और गंभीर आध्यात्मिक अर्थ धारण कर लेता है। यह चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि देवता वास्तव में हमारी मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ हैं। अधिकतर मनुष्य तो प्राणिक देवों को ही पुष्ट करने में लगे रहते हैं। वे इच्छाओं- कामनाओं, पद-प्रतिष्ठा, धन-संपदा आदि अनेकानेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। इससे ऊपर की अवस्था तब है जब व्यक्ति अपने मानसिक विचारों को पुष्ट करने के लिए अपनी ऊर्जा लगाता है। सभी प्रकार के परोपकारिता आदि के प्रचलित विचार, जैसे कि, गरीबों की और रोगियों की सेवा, मानव-कल्याण, नारी-कल्याण, या फिर देश-सेवा में आत्मोत्सर्ग करने के विचार और न जाने अन्य कितने ही ऐसे विचार इसी दायरे में आते हैं। इन सभी मानसिक प्रकार के आदशों के पीछे अपनी शक्ति लगाना मानसिक देवों की पूजा करना हुआ। इस प्रकार मनुष्य यक्षों, गंधर्वो, राक्षसों आदि की पूजा करते हैं और उनके अनुसार उन्हें फल प्राप्त हो जाता है। परंतु इन सब की बजाय जो व्यक्ति सीधे भगवान् की ओर अभिमुख होता है, उन्हीं के प्रति अपनी पूजा अर्पित करता है तो भले वह बाहरी रूप से कैसा भी अधम व्यक्ति ही क्यों न हो परंतु वह साधु मानने योग्य है क्योंकि उसमें यह संकल्प जागृत हो गया है कि भगवान् के अतिरिक्त जीवन में अन्य कुछ भी वरण करने योग्य नहीं है। और यह एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को सभी कुछ से परे उठा ले जाता है। इसीलिए हमारे सद्ग्रंथ बार-बार ऐसा कहते हैं कि जहाँ भगवान् की भक्ति से शून्य एक नैष्ठिक सात्त्विक ब्राह्मण स्वयं अपना भी उद्धार नहीं कर पाता क्योंकि वह अपनी सात्त्विकता के अहं में ही फँसा रहता है, वहीं एक पतित और अधम चेतना का व्यक्ति भी सच्चे संकल्प के जागृत होते ही अपने पूरे कुल का भी कल्याण कर देता है। हालाँकि सूक्ष्म जगत् की विभिन्न सत्ताओं और देवताओं की पूजा करते-करते भी जब व्यक्ति का कुछ विकास होता है तब उसे यह महसूस होता है कि केवल किन्हीं भौतिक, प्राणिक और मानसिक लाभों के लिए ही भगवान् की ओर मुड़ना तो एक निम्न हेतु है। यह भाव आने के बाद व्यक्ति अधिकाधिक भगवान् के अपने लिए उनकी ओर मुड़ता जाता है। कुछ का गठन इस प्रकार का होता है कि सहज ही वे भगवान् की ओर आकृष्ट रहते हैं। अब जिसमें भगवान् से मिलने की लगन है वह तो कोई भी उपाय करने के लिए तैयार रहता है। यदि कोई कह दे कि अमुक ध्यान करने से, या अमुक क्रिया करने से या फिर अन्य कोई भी उपाय करने से भगवान् की प्राप्ति हो जाएगी तो वह उसे करने के लिए तत्पर रहेगा और वैसा करने से उसे प्राप्ति हो भी जाएगी। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति जिसमें यह लगन नहीं है वह चाहे उन सारे उपायों को भी करे तो भी उसको प्राप्ति नहीं होती। इसलिए महत्त्व बाहरी क्रिया से अधिक उस आंतरिक निष्ठा और लगन का है। अतः कोई भी क्रिया साधना का अंग हो सकती है और वहीं आवश्यक नहीं कि परंपरागत रूप से शास्त्रसम्मत पद्धतियाँ भी व्यक्ति को एक पग भी आगे बढ़ा सकें। इसलिए विषय यह नहीं है कि व्यक्ति श्रीराम की पूजा करता है या शिव की या श्रीकृष्ण की या फिर देवी की। यदि व्यक्ति श्रीकृष्ण के पास इस भाव से जाए कि इससे उसकी साधना हो जाएगी, उसके जीवन में शांति आ जाएगी, उसके परिवार में सुख-शांति-समृद्धि आ जाएगी तो इस भाव में व्यक्ति भगवान् की नहीं अपितु किसी निम्न देव की ही पूजा कर रहा होता है। वहीं यदि किसी मानव गुरु के प्रति किसी में सेवा भाव, एकनिष्ठता और श्रद्धा आदि हैं तो उसके द्वारा भी वह सीधे परमात्मा की ओर ही अभिमुख होता है। इसलिए व्यक्ति किस की पूजा कर रहा है वह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, अपितु उसके पीछे जिस मनोभाव से वह अपनी पूजा अर्पित कर रहा है वही महत्त्वपूर्ण है। इसलिए जो अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए भगवान् की ओर मुड़ते हैं उस स्तर तक उन्हें उसका फल प्राप्त हो ही जाता है। परंतु वे उसी दायरे में बने रहते हैं। उससे ऊपर नहीं उठ पाते। वहीं जो किसी स्वार्थपूर्ति के लिए नहीं अपितु भगवान् के स्वयं के लिए उनकी ओर मुड़ते हैं वे सीधे भगवान् की ओर ही जाते हैं और उनके लिए निम्नतर विधान लागू नहीं होते क्योंकि वे उनसे परे चले जाते हैं।
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ।। २४।।
२४. क्षुद्र बुद्धिवाले मुझे, अव्यक्त को, अभिव्यक्ति द्वारा सीमित मानते हैं; वे मेरे अविनाशी और पूर्णतम अथवा सर्वोत्तम परं भाव को नहीं जानते।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।। २५।।
२५. और अपनी योगमाया से आवृत्त मैं सब के लिए प्रकाशित भी नहीं होता हूँ यह मोहग्रस्त अथवा मूढ़ जगत् मुझ अजन्मा और अविनाशी को नहीं जानता।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।। २६ ।।
२६. हे अर्जुन! मैं अतीत के और वर्तमान काल के और भविष्य के समस्त भूतों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता।
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ।। २७।।
२७. हे भारत! इच्छा और द्वेष से द्वंद्वात्मक'० मोह उत्पन्न होता है, और हे परंतप, उससे इस सृष्टि में समस्त भूत मूढ़ता को प्राप्त होते हैं।
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ।। २८ ।।
२८. किंतु पुण्य कर्म करनेवाले जिन मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है वे द्वंद्वजनित मोह से मुक्त होकर अपने आत्म-निवेदन में दृढ़व्रती होकर मुझे भजते हैं।
...हमारे कर्मों में सबसे पहली आवश्यकता है कि हम प्राणिक अहंकार के पाप से, काम-क्रोध की आग से, राजसिक प्रकृति की इच्छा के कोलाहल से मुक्त हो जाएँ, और ऐसा अपने नैतिक पुरुष की सात्त्विक प्रेरणा तथा प्रवृत्ति को दृढ़ करने से ही हो सकता है। जब ऐसा हो जाए, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्, - अथवा यह कहिये कि जब यह काम हो रहा हो, क्योंकि एक बिंदु के बाद सात्त्विक प्रकृति में समस्त वृद्धि उच्च शान्ति, समता और त्रिगुणों से अतिक्रमण की अधिकाधिक क्षमता ले आती है, तभी - द्वन्द्वों के ऊपर उठकर निर्व्यक्तिक, सम, अक्षर ब्रह्म के साथ एकात्म, सब भूतों के साथ एकीभूत हो जाना आवश्यक है। आत्मस्वरूप में वर्धित होने की यह प्रक्रिया हमारे शुद्धिकरण को पूरा कर देती है। पर जिस समय यह प्रक्रिया जारी हो, जब जीव आत्मज्ञान में परिवर्धित हो रहा हो, उस समय उसे भक्ति में भी परिवर्धित होना होता है.... एक बार समत्व और एकत्व दृष्टि पूर्णरूप से प्राप्त हो जाए, ते द्वन्द्वमोहविनिर्मुक्ताः, तो परा भक्ति, भगवान् के प्रति सर्वभावेन प्रेम-भक्ति ही जीव का संपूर्ण और एकमात्र धर्म बन जाती है। अन्य सभी धर्म उस एक शरणागति में लय हो जाते हैं, सर्वधर्मान्परित्यज्य। तब जीव इस भक्ति में तथा अपनी संपूर्ण सत्ता के, ज्ञान और कर्म के आत्मोत्सर्ग के व्रत में दृढ़ हो जाता है; क्योंकि अब उसे अपने सुदृढ़ आधार के लिए, अपने अस्तित्व और अपने कर्म के चरम आधार के लिए सर्व-प्रवर्तक भगवान् का पूर्ण, समग्र और एकीकारी ज्ञान प्राप्त होता है, ते भजन्ते मां दृढ़व्रताः।
-------------------------------------------
"[हमारी निम्न जीव-प्रकृति की मुख्य चार ग्रंथियों में से एक द्वंद्व है।... गीता में हमारे लिये इनका निर्देश किया गया है और इन पर बड़े बलपूर्वक तथा निरन्तर, प्रबल शब्दों में एवं बारम्बार आग्रह किया गया है; ये... ग्रंथियाँ हैं कामना, अहंकार, द्वंद्व और प्रकृति के तीन गुण; क्योंकि गीता के विचार में मुक्त होने का अर्थ है निष्काम और निरहंकार होना, मन, अन्तरात्मा और आत्मा में सम तथा त्रिगुण से रहित, निबैगुण्य, होना।
प्रश्न : आत्मज्ञान में परिवर्धित होने की प्रक्रिया में भक्ति में भी परिवर्धित होने पर बल क्यों दिया गया है?
उत्तर : यदि सच्चा आत्मज्ञान है तो भक्ति आएगी ही। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं आ सकता। संसार में जो तथाकथित ज्ञानी हैं उनके ज्ञान का आकलन हम उनमें भक्ति की मात्रा से कर सकते हैं। यदि वे भक्ति शून्य हैं तो वे बिल्कुल कोरे हैं। इसी प्रकार यदि कोई स्वयं को भगवान् का भक्त समझता है पर ज्ञान-शून्य है तो उसकी भक्ति अधकचरी है। भक्ति जब एक सीमा को लाँघ जाती है तब वह आवश्यक रूप से सच्चा ज्ञान लाती ही है। इसलिये भक्ति से आरंभ करने पर ज्ञान आ जाता है और ज्ञान से आरंभ करने पर भक्ति स्वयं ही आ जाती है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गीता इसी बात को समझाने के लिए यह सामने ला रही है कि जो पापी नहीं है वह तो दृढ़ होकर भगवान् की भक्ति करेगा ही। पापी मनुष्य में तो ज्ञान आना संभव ही नहीं है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यही है कि भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है और कर्म का आधार है। बिना भगवान् की भक्ति हुए उनके लिए कर्म करना संभव नहीं है। किसी व्यक्ति के प्रति लगाव होने पर ही हम उसके लिए कर्म कर सकते हैं अन्यथा नहीं। अतः भक्ति कर्मों का आधार है और ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान भक्ति में आकर समाहित हो जाता है। किसी को आरंभ में ज्ञान का कुछ आभास हो सकता है परन्तु यदि उसके अन्दर भक्ति की भावना नहीं है तो उसका ज्ञान कोरा और निरर्थक है। कर्मयोग में भी यदि भक्ति नहीं हो तो कर्म भी कोई उपयोग के नहीं होते। संसार में कितने लोग हैं जो घोर परिश्रम करते हैं परंतु इससे कर्मयोग या फिर उनकी साधना नहीं हो जाती। यदि व्यक्ति के अन्दर भक्ति नहीं है तो उसके कर्म योग न होकर एक प्रकार से रोग ही होते हैं।
प्रश्न : क्या पहले एकत्व और समत्व के आने पर परा-भक्ति आती है?
उत्तर : चीजों को रखने का गीता का अपना एक क्रम है, निरूपण की एक पद्धति है। क्योंकि अपनी शिक्षा का निरूपण करने के लिए उसे एक क्रम अपनाने की आवश्यकता है। परंतु भगवान् की सत्ता अनंत है और अपनी अभिव्यक्ति में वह किसी भी तय क्रम के अनुसार चलने को बाध्य नहीं है। और न ही ऐसा है कि कोई तय क्रम है जिसमें कि सभी गुणों को या तत्त्वों को एक के बाद एक आना है। ये सभी चीजें तो समझाने के लिए ही हैं ताकि हमारी बुद्धि इन सूक्ष्म विषयों के बारे में कुछ समझ सके। इससे अधिक इन सब बातों की उपयोगिता नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका विकासक्रम विशिष्ट प्रकार का होता है। इतना भर कहा जा सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके साथ लगभग समान होती हैं। परंतु वास्तविक अभिव्यक्ति में सब कुछ व्यक्तिविशेष के अनुसार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए साधना में सामान्य धारणा है कि पहले प्रकृति को तैयार करना होता है तब व्यक्ति को सूक्ष्म या फिर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। परंतु श्रीअरविन्द ने कहा कि उनके लिए क्रम इससे उल्टा था। उन्हें अनुभव पहले हुए और प्रकृति उसके बाद तैयार हुई। क्योंकि उनका कहना है कि किसी न किसी भाग में पहले अनुभव हुए बिना प्रकृति तैयार नहीं हो सकती। इसलिए इन चीजों के विषय में पढ़ते समय या फिर इनका वर्णन सुनते समय व्यक्ति में इतनी समझ होनी चाहिये और विवेक होना चाहिये कि किसी निरूपण विशेष के लिए ही वह क्रम आवश्यक है अन्यथा वास्तविक अभिव्यक्ति में चीजें भिन्न रूप से हो सकती हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर्वमान्य हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब तक प्रकृति एक सीमा तक तैयार नहीं हो जाती तब तक एक सीमा से बाहर के अनुभव होना कठिन है। परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि यदि व्यक्ति को वे अनुभव प्राप्त हो जाते हैं तो उनके परिणामस्वरूप उसकी प्रकृति भी तैयार हो जाएगी। क्योंकि अनुभवों का प्रवाह, उनकी प्रगाढ़ता, उनका स्तर जितना ही तीव्र और उच्च होगा उतनी ही शीघ्र प्रकृति की तैयारी होगी। गीता अपना निरूपण एक शैली विशेष में करती है क्योंकि किसी एक शैली का अनुसरण किये बिना तो कोई निरूपण करना मुश्किल है। आरंभ में तो भक्ति अप्रकट रूप से केवल मन का एक भाव मात्र होती है और बाद में धीरे-धीरे वह बढ़ती जाती है और प्रकट रूप अपना कर अपना सच्चा स्वरूप अपनाती जाती है। गीता इसी तत्त्व का क्रमबद्ध रूप से निरूपण करती है। पहले वह कर्म से आरम्भ करती है और बाद में उसमें ज्ञान को समाविष्ट करती है। ज्ञान और कर्म का निरूपण और समन्वय करने के बाद वह उसमें भक्ति तत्त्व का समावेश करके नौवें अध्याय में तीनों तत्त्वों का समन्वय साधती है। परंतु वर्तमान में वह ज्ञान और भक्ति का समन्वय साध रही है। गीता कहती है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह भगवान् की भक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। भगवान् ने चार प्रकार के भक्त बताए हैं - आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी – परंतु इनमें ज्ञानी को बाकी तीनों से श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि वह भगवान् के निजस्वरूप को तत्त्वतः जानता है और उसी कारण वह उनसे प्रेम करता है और उनकी भक्ति करता है जिस कारण उसे जीवन की अन्य सब चीजें व्यर्थ प्रतीत होती हैं। और यह भाव बाहरी रूप से जो घोर पाप में लिप्त है उसके अंदर भी उदित हो सकता है और इसके हमें अनेकानेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जगाई-मधाई के प्रसंग में हम देखते हैं कि किस प्रकार पापाचरण के अलावा कोई दूसरा व्यवहार तो वे जानते ही नहीं थे और फिर भी भगवान् की कृपा से हृदय परिवर्तन होने के कारण वे परम् भक्त बन गए। इसलिए इन सब चीजों का कोई अपरिहार्य बाहरी या मानसिक तर्क या विधान नहीं है। सामान्य तौर पर तो ऐसा हृदय परिवर्तन या ऐसा भाव उन लोगों में उदित होता है जिन्होंने सुकृत कर्म किए हों परंतु यह कोई ऐसा अटल नियम नहीं है जिसके कि अपवाद न होते हों। इन सभी चीजों के कोई तय मानसिक नियम नहीं बनाए जा सकते। इनका अपना एक सूक्ष्म या गहरा कारण होता है जो कि बुद्धि से परे है।
आखिर ज्ञान है क्या? सामान्यतः हम जिसे ज्ञान कहते हैं वह ज्ञान नहीं केवल मानसिक रूप से कुशल होना हो सकता है या अधिकांशतः तो वह केवल मानसिक उग्रता या हलचल ही होती है। सही ज्ञान के अंदर तो हृदय का अन्तर्ज्ञान सम्मिलित होता है। भले सतह पर व्यक्ति किसी चीज का क्यों और कैसे न जानता हो परंतु हृदय में उसे एक पक्का आभास होता है कि सही चीज क्या है। और यही सही ज्ञान है। जिसे हम मन (Mind) कहते हैं उसके दो केन्द्र होते हैं - हृदय और बुद्धि। इन दोनों में भी हृदय का केन्द्र अधिक प्रबल है। हृदय को अंतर्बोध प्राप्त होता है जो जानता है कि सही चीज क्या है। और यही महत्तर और महत्त्वपूर्ण ज्ञान है। जो भी व्यक्ति भगवान् के मार्ग पर चलता है उसे अवश्य ही गहरा अंतर्ज्ञान होता है तभी तो वह उस मार्ग का अनुसरण करता है अन्यथा तो वह उस मार्ग का वरण ही न करता। परंतु चूंकि ज्ञान की हमारी परिभाषा सामान्यतः भिन्न होने के कारण हम उसे ज्ञान नहीं कहते। जबकि ऐसे व्यक्ति को गहराई में सच्चा ज्ञान अवश्य होता है तभी तो वह सही पथ का वरण और अनुसरण करता है। सच्चे दृष्टिकोण से मूढ़ तो वे हैं जिन्हें इस गहरे सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ जिस कारण वे जीवन के प्रपंचों में ही लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए कहने को व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो परंतु वह पेड़ की उसी डाली को काटने का प्रयास कर रहा हो जिस पर वह बैठा है तो इसे ज्ञान कैसे कह सकते हैं। उसी प्रकार जो आत्मा हमारे अस्तित्व का संपूर्ण आधार है उसी की हम उपेक्षा करते हों और फिर भी सुखी होने की चेष्टा करते हों तो यह ज्ञान कैसे हो सकता है। जब आत्मा ही हमारा सच्चा स्वरूप है, हमारा सच्चा 'स्व' है तो उसकी ओर आकृष्ट होना तो सहज ही है, और ऐसा करना सच्चे ज्ञान का द्योतक है। यदि व्यक्ति के अन्दर थोड़ा भी ज्ञान है तो उसे समझ में आ जाएगा कि जीवन को व्यर्थ गँवाने की अपेक्षा उसे परमात्मा की ओर मोड़ना ही उसे औचित्य प्रदान करता है।
प्रश्न : इसमें बताया गया है कि नैतिक पुरुष की सात्त्विक प्रेरणा तथा प्रवृत्ति को दृढ़ करने से हम प्राणिक अहंकार के पाप से, काम-क्रोध की आग से, राजसिक प्रकृति की इच्छा के कोलाहल से मुक्त हो जाते हैं। तो नैतिक पुरुष की प्रेरणा से क्या तात्पर्य है?
उत्तर : अलग-अलग समाज के अलग-अलग नैतिक विधान होते हैं। कुछ नैतिक विधान वेदान्त के सत्य पर आधारित हैं, जैसे कि, चूंकि सभी के अंदर एक ही आत्मा है और कोई दो हैं ही नहीं इसलिए सभी के साथ अपना समझकर व्यवहार करना चाहिये, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिये। अधिकांशतः तो इसी वैदान्तिक सत्य के आधार पर अनेक नैतिक विधानों का निर्माण हुआ है। अन्य कुछ अधिक बाहरी नैतिक विधान हैं जैसे कि भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, जीवनचर्या कैसी होनी चाहिये, आदि-आदि। और इस प्रकार के नैतिक विधान तो समाज में देश, काल के अनुसार बदलते रहते हैं। परंतु कुछ विधान जो वेदान्त के मूल सत्यों पर आधारित होते हैं उनका खंडन करना अपने अस्तित्व के मूल सत्यों का ही खंडन करना हुआ व अपने विनाश की ओर कदम बढ़ाना हुआ। उदाहरण के लिए यह विचार कि 'दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिये' एक मूलभूत सत्य पर आधारित बात है क्योंकि मूल रूप से सभी में एक ही सत्ता है इसलिए भेदभाव करना तो उस सत्य का खंडन करना हुआ। अब यदि व्यक्ति दूसरे जीवों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो भले ही वह इस कृत्य को उचित ठहराने के लिए किन्हीं भी नैतिक बातों का सहारा ले परंतु यह तो मूल सत्य से बिल्कुल विसंगत बात है। अब मनुष्यजाति बिना सोचे-समझे अपनी क्षुद्र तृष्णाओं की पूर्ति के लिए पशुओं के साथ जिस घोर निर्दयता का व्यवहार करती है उसमें किसी प्रकार की कोई नैतिकता का तो कोई लेश मात्र भी नहीं है। परंतु उसी नैतिकता की हम दुहाई देने लगते हैं जब हम पर कोई अत्याचार करता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है। उत्तरी अमरीकी भारतीयों (North American Indians) को यह सहज बोध था कि अनेक व्यक्ति मिलकर यदि किसी एक पशु पर हमला करें तो यह अनुचित बात है। वे लड़ाई में उस पशु को भी बराबर का मौका देना चाहते थे और यदि वह पशु उन्हें मार डाले तो भी इसे गलत नहीं मानते थे। इस प्रकार उनके नैतिक विधान बिल्कुल भिन्न प्रकार के थे। हालाँकि वास्तव में तो अपने आप में नैतिकता कोई महत्त्वपूर्ण चीज नहीं है, इसका केवल इतना उपयोग है कि यह घोर बर्बरता पर कुछ अंकुश लगा सकती है परंतु अधिकांशतः तो यह अपने कृत्यों को उचित ठहराने के लिए, अपने गलत कामों को सही बताने के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। जिस प्रकार का व्यवहार मनुष्यजाति पशुओं के साथ करती है उसका आकलन यदि किसी पशु के दृष्टिकोण से किया जाए तो कदाचित् ही वह मनुष्यों के पक्ष में कोई नेक बात सोची जा सकती है। इसीलिए गीता एक स्थान पर कहती है 'सर्वभूत हिते रताः' अर्थात् जो सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहता है वही मुझे प्राप्त करता है। इसमें किसी जीव विशेष के कल्याण की बात नहीं है अपितु समस्त जीवों के कल्याण की बात है। एक सच्चे दृष्टिकोण में नैतिकता तो वह है जो परमात्मा की इच्छा हो। उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना ही सच्ची नैतिकता है। जब व्यक्ति उस चेतना में होगा तभी वह सभी जीवों का कल्याण कर सकता है और सच कहें तो वह कल्याण करने के भाव से ऐसा कोई कार्य नहीं करता। वह तो भगवद् इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए कार्य करता है और उसके परिणामस्वरूप सभी जीवों का स्वतः कल्याण होता है। यदि हमारे मानवीय नैतिक आदर्शों के अनुसार सोचें तो महाभारत का युद्धकर्म किन्हीं भी मानदंडों पर नैतिक नहीं हो सकता। परंतु फिर भी चूँकि वही श्रीभगवान् की निहित इच्छा थी इसलिए उसे चरितार्थ करना ही सच्ची नैतिकता थी। यदि नैतिक विधान आध्यात्मिक विधानों के विपरीत हों तो उनका कोई मूल्य नहीं है। उनका मूल्य तो केवल तभी है जब वे गहरे आंतरात्मिक विधानों को चरितार्थ करने में सहयोग करें। अवश्य ही घोर पाशविकता में पड़े व्यक्ति के लिए समाज के कुछ विधान उस पर कुछ अंकुश लगाने का काम कर सकते हैं और उतनी ही उनकी उपयोगिता है।
प्रश्न : हमारी निम्न जीव-प्रकृति की ये मुख्य चार ग्रंथियाँ क्या हैं?
उत्तर : जैसा कि गीता ही बताती है कि ये ग्रंथियाँ हैं कामना, अहंकार, द्वंद्व और प्रकृति के तीन गुण। इनमें कामना और अहंकार तो आत्मपरक अर्थात् पुरुष पक्ष की ग्रंथियाँ हैं और द्वंद्व और गुण प्रकृति पक्ष की ग्रंथियाँ हैं। व्यक्ति यदि कामना के वशीभूत होकर किसी चीज को देखता है तो वह उसे सही रूप में नहीं देख पाएगा। कामना का आधार है अहं। यदि अहं न हो तो कामना नहीं हो सकती। यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो सुख का अनुभव होता है और यदि वह पुष्ट नहीं होती तो उसकी अपनी प्रतिक्रियाएँ होती हैं। इस प्रकार कामना और अहंकार हुई पुरुष पक्ष की ग्रंथियाँ और प्रकृति पक्ष में हैं द्वंद्व और त्रिगुण। भौतिक प्रकृति में शीत-ऊष्ण आदि द्वंद्व होते हैं, राजसिक प्रकृति में प्रिय-अप्रिय आदि द्वंद्व होते हैं और सात्त्विक प्रकृति में उचित-अनुचित आदि द्वंद्व होते हैं। साथ ही भौतिक प्रकृति तमस् प्रधान होती है, प्राणिक प्रकृति रजस् प्रधान होती है और मानसिक प्रकृति सत्त्व प्रधान होती है। प्रत्येक व्यक्ति में तीनों ही प्रकृतियाँ होती हैं परंतु अंतर इनकी प्रधानता में होता है। इस प्रकार द्वन्द्वों और तीनों गुणों से सारे संसार का खेल चलता रहता है। यदि व्यक्ति अतिशय रूप से तामसिक है तो भी उसका नाश निश्चित है और अतिशय रूप से राजसिक है तो भी, क्योंकि यदि व्यक्ति में इच्छाएँ-कामनाएँ आदि एक सीमा से अधिक प्रबल हैं तो भी व्यक्ति उन्हें सहन नहीं कर सकता और उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। शरीर और प्राण के भड़के हुए आवेगों को तुष्ट करने की चेष्टा में ही तो हम व्यक्तियों को अपना संतुलन खोते देखते हैं। और यह चीज हमें पश्चिमी संस्कृति में अधिक दिखाई देती है क्योंकि वहाँ इन वृत्तियों पर अंकुश लगाने वाले आध्यात्मिक प्रभाव का बहुत कुछ अभाव है जबकि भारत में आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण बहुत कुछ बचाव हो जाता है। परंतु फिर भी व्यक्ति द्वन्द्वों से मुक्त नहीं हो सकता। सात्त्विक प्रकृति वाले मनुष्य में द्वन्द्वों के प्रति सहनशीलता थोड़ी बढ़ जाती है। हालाँकि तकलीफ तो उसे होती ही है परन्तु उसकी सहन करने की सामर्थ्य राजसिक और तामसिक व्यक्ति की अपेक्षा बढ़ जाती है। राजसिक व्यक्ति को सात्त्विक व्यक्ति से अधिक और तामसिक व्यक्ति को सबसे अधिक कष्ट होता है। गीता इन्हीं चार ग्रंथियों को सुलझाने के ऊपर सबसे अधिक बल देती है क्योंकि इन्हीं से यह सारा विश्व प्रपंच चलता रहता है। इनमें भी कामना से मुक्त होने पर गीता सर्वाधिक बल देती है। कामना अहं के कारण होती है। अहं से मुक्त होने के दो ही उपाय हैं- या तो अहं मुक्त चेतना हमारे अंदर अवतीर्ण हो या फिर भक्ति की प्रगाढ़ता हो। जब भक्ति प्रगाढ़ हो तब भले ही व्यक्ति को अपने पृथक् अस्तित्व का भान हो तब भी अहं का जो विष है वह नहीं रहता। श्री रामकृष्ण जी इसको समझाने के लिए जली हुई रस्सी का रूपक देते थे। वे कहते थे कि जिस प्रकार जली हुई रस्सी में किसी चीज को बाँधने की सामर्थ्य नहीं होती उसी प्रकार भक्ति आने से अहंकार का विष खत्म हो जाता है और व्यक्ति चीजों को जिस प्रकार अहमात्मक चेतना से देखकर दूषित करता था वह अब नहीं रहता। भक्ति अपने साथ सारे गुण और अच्छी चीजें ले आती है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ सत्य, ज्ञान आदि चीजें अपने आप ही आ जाती हैं।
प्रश्न : दृढ़ रूप से भक्ति किसकी की जाए?
उत्तर : सच्चे भाव में इस प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह प्रश्न तो उनके मन में उठ सकता है जो नाम तो भक्ति का लेते हैं परंतु मन में यह सौदेबाजी ही रहती है कि किसकी भक्ति करने से सर्वाधिक लाभ होगा। हृदय का भाव तो बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है। वह मानसिक तर्क के आधार पर नहीं चलता। इसलिए यह तो हृदय पर निर्भर करता है कि वह किसके प्रति समर्पित हो जाए। भक्ति तो किसी के प्रति भी हो सकती है फिर चाहे वह दूसरों की दृष्टि में पूजा का छोटा ही पात्र क्यों न हो। इसलिए दृढ़ भक्ति तो अन्तर की गहराइयों से ही आ सकती है। यह बाहर से प्रयत्न करने पर नहीं आती। जैसे, जब पार्वती जी भगवान् शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थीं तो कुछ ऋषियों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके समक्ष शिवजी को उनके लिए बिल्कुल अनुपयुक्त वर बताकर विष्णु जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। परन्तु पार्वती जी तो अपने मन में अनन्य रूप से भगवान् शिव को ही वरण कर चुकी थीं इसलिये उन्होंने सभी प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि भले ही भगवान् विष्णु शिव से बहुत श्रेष्ठ हो सकते हैं परन्तु उनका मन तो भगवान् शिव में ही रम गया है इसलिए या तो वे उन्हीं का वरण करेंगी या फिर आजीवन कँवारी रहना पसंद करेंगी। अतः प्रेम बाहरी रूप से सोच-समझकर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भक्ति भी बुद्धि से सोच समझकर नहीं की जा सकती।
प्रश्न : तब फिर ज्ञान की क्या उपयोगिता है और ज्ञान के साथ भक्ति कैसे जुड़ेगी?
उत्तर : वास्तव में सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति तो दोनों साथ-साथ ही चलते हैं। बिना भक्ति के सच्चा ज्ञान आता ही नहीं। भगवान् के सत्स्वरूप के बोध को ही तो ज्ञान कहते हैं और जब व्यक्ति को भगवान् से कोई प्रेम न हो तो उसे ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे को सुदृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रीकृष्णप्रेम कहते थे कि जो व्यक्ति कहता है कि वह जानता तो है परन्तु प्रेम नहीं करता तो इसका अर्थ है कि वह जानता नहीं, और जो कहता है कि वह प्रेम तो करता है परंतु जानता नहीं है तो वह प्रेम नहीं करता। इसलिए जो यह कहता है कि वह बहुत बड़ा भक्त है पर यदि उसमें ज्ञान नहीं है, तो उसमें भक्ति भी नहीं है। गीता में भगवान् बार-बार कहते हैं कि वही मुझे समग्र रूप से जानता है जो मेरा भक्त है। ग्यारहवें अध्याय में भगवान् अर्जुन को अपना विश्वरूपदर्शन कराते हुए कहते हैं कि 'न ज्ञान से, न कर्म से, न तपस्या से, न यज्ञ से, न दान आदि से मेरे इस रूप के दर्शन किए जा सकते हैं, केवल भक्ति के द्वारा मेरे इस रूप को देखा जा सकता है।' इसलिए जिसमें ज्ञान है उसमें भक्ति आएगी और जिसमें भक्ति होगी वह परमात्मा के लिए कर्म भी करेगा। ये तीनों ही चीजें एक साथ गति करती हैं।
इस प्रकार आध्यात्मिक विकास के द्वारा भक्ति ज्ञान के साथ एक हो जाती है। जीव एकमेव भगवान् में आनन्द लाभ करता है, - उन भगवान् में जिन्हें अखिल सत्, चित् और आनन्द के रूप में, सब पदार्थों, प्राणियों और घटनाओं के रूप में जाना जाता है, जिन्हें प्रकृति में, पुरुष में, और प्रकृति और पुरुष के परे जो है उनके रूप में जाना जाता है। वह नित्य ही भगवान् के साथ सतत् युक्त है, नित्ययुक्त; उसका संपूर्ण जीवन और उसकी सत्ता उन परम् के साथ सनातन योग से युक्त है जिनके परे, जिनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, उन विश्वात्मा के साथ युक्त है जिनके अतिरिक्त और कोई नहीं, कुछ भी नहीं। उसकी सारी भक्ति उन्हीं एक पर केन्द्रित है, एकभक्तिः, किसी आंशिक देवता, विधि-विधान या संप्रदाय पर नहीं। यह अनन्य भक्ति ही उसके जीवन का संपूर्ण विधान है और वह सब धार्मिक मत-मतांतरों, आचारों और जीवन के वैयक्तिक उद्देश्यों से परे जा चुका है। उसे कोई दुःख नहीं हैं जो दूर करने हों, क्योंकि वह सर्वानन्दमय परमात्मा को पा चुका है। उसकी कोई इच्छाएँ नहीं हैं जिनके पीछे वह भटकता फिरे, क्योंकि वह उच्चतम और 'सर्व' को पा चुका है, और वह उस सर्व-शक्ति के सन्निकट है जो पूर्ण परितृप्ति प्रदान करती है। उसके कोई संशय या भ्रमित खोजें नहीं बची, क्योंकि उस पर सारा ज्ञान उस ज्योति से प्रवाहित होता है जिसमें वह निवास करता है। वह पूर्ण रूप से भगवान् से प्रेम करता और भगवान् का प्रिय होता है; क्योंकि जैसे वह भगवान् में हर्ष लेता है वैसे ही भगवान् भी उसमें आनन्द लेते हैं। यही वह ज्ञान से युक्त भगवत्प्रेमी है, ज्ञानी भक्त है।
vii. 17
यदि कोई व्यक्ति आपके सच्चे रूप को पहचानता हो तो वह आपके किन्हीं भी बाहरी रूप-रंग से भ्रमित नहीं होने वाला भले ही आप कितने भी भेष क्यों न बदल लें और चूंकि वह आपके हर रूप में आप को जानता है इसलिए वह किसी भी रूप में आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करने वाला। कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति में भक्ति ज्ञान के साथ एक हो जाती है तब वह सभी आवरणों के पीछे केवल परमात्मा का ही रूप देखता है। इसीलिए गीता में भगवान् कहते हैं कि 'मम माया दुरत्यया' अर्थात् 'मेरी माया को अतिक्रम करना कठिन है'। केवल वे ही इससे ऊपर उठकर उनको जान सकते और उनके पास जा सकते हैं जो उनकी भक्ति कर के उनको भजते हैं। और जब व्यक्ति उन्हें तत्त्वतः जान जाता है तब उसे संसार की किसी चीज से मोह या घृणा भी नहीं होते। साथ ही व्यक्ति अपने दुःखों और सुखों से भी ऊपर उठ जाता है क्योंकि सुख-दुःख और कुछ नहीं केवल भिन्न रूप मात्र ही हैं जिनमें भगवान् हमसे आकर मिलते हैं। जब वे किसी एक प्रकार के वस्त्रों में आकर हमसे मिलते हैं तो उसे हम अभ्यासवश सुख कह देते हैं और यदि दूसरे परिधान में आ जाएँ तो उसे दुःख कह देते हैं। अब चूंकि हमें वस्तुओं की प्रतीति के पीछे के सत्य का कोई ज्ञान नहीं होता इसलिए हम भिन्न चीजों के प्रति भिन्न-भिन्त्र मनोभाव अपना लेते हैं और उन पूर्वाग्रहों के अनुसार ही चीजों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। पर जब हमें वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तब वस्तुओं के प्रति हमारा सारा मनोभाव ही बदल जाता है और हम यह भी जान सकते हैं कि चीजों के पीछे परमात्मा किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा जानकर हम उनके संकल्प की अभिव्यक्ति में रोड़ा न डालकर सहयोग करने का भाव अपना लेते हैं। अतः सच्चा ज्ञान होने पर तो सुख-दुःख का नहीं बल्कि सब कुछ आनन्द का विषय बन जाता है। जब तक परमात्मा से हमारा किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हो जाता तब तक हम उनके विषय में शंकित ही रहते हैं और छोटी सी घटना से भी विचलित हो उठते हैं। परंतु जैसे हम अपने अंतरंग मित्र की क्रियाकलाप से कभी शंकित नहीं होते बल्कि हमें दृढ़ विश्वास होता है कि वह हमारे हित के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता वैसे ही जब परमात्मा के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है और हम उस चेतना में निवास करने लगते हैं तब हम स्वच्छंद और निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हमें यह आश्वासन होता है कि सर्वत्र केवल भगवान् ही हैं इसलिए किसी प्रकार के कोई भय, संकोच आदि की कोई आवश्यकता नहीं। जब व्यक्ति को सर्वत्र जगज्जननी के दर्शन होते हैं तब एक बालक की भाँति वह निर्भय रूप से विचरण करता है और बिल्कुल निश्चिंत और आनंदमग्न रहता है।
हमारे आत्मसमर्पण में समग्र ज्ञान का होना उसकी प्रभावशाली शक्ति की पहली शर्त है। और इसलिए हमें सबसे पहले इस पुरुष को, तत्त्वतः, अर्थात् उसकी दिव्य सत्ता की सभी शक्तियों और तत्त्वों में, इसके संपूर्ण सामंजस्य में, इसके सनातन विशुद्ध स्वरूप तथा जीवनलीला में जानना होगा। परन्तु प्राचीन चिंतन की दृष्टि में इस तत्त्वज्ञान का सारा मूल्य बस इस मर्त्य जीवन से मुक्त होकर एक परम् जीवन के अमृतत्व को प्राप्त करने की शक्ति में ही निहित था। इसलिए गीता आगे अब यह दर्शाने की ओर अग्रसर होती है कि यह मुक्ति भी किस प्रकार, अपने उच्चतम अंश में, गीता को अपनी आध्यात्मिक आत्मपरिपूर्णता की साधना का एक परम् फल है।
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ।। २९।।
२९. मुझमें आश्रय ग्रहण करके जो लोग अपने आध्यात्मिक प्रयास को जरा और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने की ओर लगाते हैं वे उस ब्रह्म (तद् ब्रह्म) को और समग्र अध्यात्म प्रकृति को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं।
यहाँ गीता के कथन का यही आशय है कि पुरुषोत्तम का ज्ञान पूर्ण ब्रह्मज्ञान है।
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।। ३०॥
३०. क्योंकि वे मुझे जानने के साथ-ही-साथ अधिभूत (भौतिक प्रकृति) को और अधिदैव (दैवी प्रकृति) को और अधियज्ञ (यज्ञ के स्वामी के सत्य) को भी जानते हैं, वे लोग भौतिक जीवन से प्रयाण के कठिन समय में भी मेरा ज्ञान बनाए रखते हैं और उस घड़ी में भी अपनी संपूर्ण चेतना मेरे साथ युक्त किये हुए रहते हैं।
अतः वे मुझे प्राप्त होते हैं। मर्त्य-जीवन से छूटकर वे भगवान् के उस परम् पद को उतनी ही सफलता के साथ पाते हैं जितनी सफलता से वे लोग जो अपने पृथक् व्यष्टिभाव को निर्गुण अक्षर ब्रह्म में घुला-मिला देते हैं। इस प्रकार गीता इस महत्त्वपूर्ण और निर्णायक सप्तम अध्याय को समाप्त करती है।
इस प्रकार सातवाँ अध्याय 'ज्ञानविज्ञानयोग' समाप्त होता है।
परिशिष्ट
भागवत् अवतारों का रहस्य
....इस बात को समझाना बड़ा आसान है कि किस प्रकार वह व्यक्ति, जिसे यह अनुभव प्राप्त है, इसे फैला सकता है, दूसरों पर क्रिया कर सकता है; क्योंकि यह अनुभव प्राप्त करने के लिये तुम्हें एकमेव का, समस्त अभिव्यक्ति के परमोच्च सारतत्त्व का, परम उद्गम और परम साररूप का, जो कुछ भी है उस सब के परम स्रोत और सत्स्वरूप का स्पर्श करना होगा; और एकाएक ही तुम परम ऐक्य के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हो - तब फिर व्यक्तियों का कोई पार्थक्य नहीं रहता, एकमात्र एक ही स्पन्दन रहता है जो बाह्य रूप में अनिश्चित काल तक दुहराया जा सकता है...यह एकमात्र स्पंदन सर्वत्र स्थितिशील (static) होता है, परंतु जब कोई इसे सचेतन रूप से अनुभूत कर लेता है, तब उस व्यक्ति के पास उसे जहाँ कहीं भी वह उसे निर्देशित करे वहीं उसे क्रियाशील करने की शक्ति होती है; कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति किसी चीज को हिलाता-डुलाता नहीं है, परंतु जहाँ कहीं भी वह अपनी चेतना को निर्देशित करता है वहाँ चेतना का दबाव ही उसे सक्रिय कर देता है।
यदि तुम काफी ऊँचे उठ जाओ तो तुम अपने-आप को समस्त पदार्थों के केंद्र में पाते हो। और जो कुछ इस केंद्र में अभिव्यक्त है वह सब वस्तुओं में अभिव्यक्त हो सकता है। यही महान् रहस्य है, व्यष्टिगत रूप में भागवत् अवतार का रहस्य, क्योंकि सामान्यतया यह होता है कि जो कुछ केन्द्र में अभिव्यक्त होता है वह बाह्य रूप में तब अनुभूत या मूर्त होता है जब वैयक्तिक रूप में संकल्प-शक्ति जाग उठती है और प्रत्युत्तर देती है। जबकि, यदि केन्द्रीय 'संकल्प' एक व्यष्टिगत सत्ता में सतत् और स्थायी रूप में प्रकट होता है तो यह व्यष्टि-सत्ता इस 'संकल्प' तथा दूसरे व्यक्तियों के बीच एक मध्यस्थ का काम कर सकती है और उनके लिये भी संकल्प कर सकती है। यह व्यष्टि-सत्ता जो कुछ देखती है या अनुभव करती है और अपनी चेतना में सर्वोच्च संकल्प को अर्पित करती है वह सब इस प्रकार उत्तरित (answered) हो जाता है मानो वह वस्तु प्रत्येक व्यक्ति से आई हो। और यदि किसी कारण उन व्यष्टिगत तत्त्वों का उस प्रतिनिधि सत्ता के साथ थोड़ा-बहुत सचेतन या ऐच्छिक संबंध हो तो उनका संबंध प्रतिनिधि सत्ता की प्रभावोत्पादकता को, उसकी कार्यसाधकता को बढ़ा देता है; और इस प्रकार परम कर्म या परम प्रभाव जड़तत्त्व में अधिक ठोस और स्थायी रूप में कार्य कर सकता है। यही चेतना के इन अवरोहणों का कारण है - जिसे हम "ध्रुवीकृत" (polarised) चेतना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अवरोहण पृथ्वी पर सदा किसी निश्चित उद्देश्य और किसी विशेष उपलब्धि और किसी विशिष्ट कार्य के लिये आते हैं एक ऐसे कार्य के लिए आते हैं जो अवतार ग्रहण से पूर्व ही नियत और निर्धारित किया जा चुका होता है। ये कार्य पृथ्वी पर सर्वोच्च अवतारों के महान् सोपान होते हैं।
श्रीमाँ ने यहाँ पर्दा हटा कर पूरा रहस्य ही उद्घाटित कर दिया है। यही भागवत् व हमारे अन्य पुराणों में लिखी अवतार विषयक बातों के पीछे का सत्य है। यही क्रिया श्रीअरविन्द आश्रम, पांडिचेरी में चरितार्थ हुई। ऐसे-ऐसे लोग जिनका साधना से, आध्यात्मिकता से कोई सरोकार तक नहीं था वे भी श्रीमाँ व श्रीअरविन्द के साथ जुड़ गए और आध्यात्मिक पथ पर बहुत विकसित हुए।
इस बात का श्रीअरविन्द ने भी संकेत तो दिया था परन्तु उन्होंने स्पष्ट रूप से इस तरीके से इस बात को नहीं कहा। श्रीमाँ ने यहाँ जिसका वर्णन किया है उसका अन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, हाँ, हमारे पुराणों में यह निहित अवश्य है। भागवत् में भी इसका उल्लेख है कि जो लोग भगवान् के सम्पर्क में आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। वे तो भगवान् के संपर्क मात्र से ही उच्च स्थिति में पहुँच जाते हैं। यह कैसे होता है? श्रीमाँ हमें बताती हैं कि भगवान् जब सशरीर विद्यमान होते हैं तब उनके सम्पर्क से हमारी सत्ता में जो सत्य छिपा रहता है वह ऊपर आ जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया श्रीमाँ ने बताई है। और यदि इसमें कोई प्रक्रिया न भी हो तो भी उनकी उपस्थिति का प्रभाव इतना होता है कि यदि उनसे हमारा सीधा सम्बन्ध न भी हो तो भी वे चाहे सो कर सकते हैं। वहीं यदि उनके साथ सीधा संबंध हो तब वे अत्यंत प्रभावशाली रूप से क्रिया कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होने पर ही क्रिया करते हों। अवतार की इस प्रक्रिया द्वारा उनका प्रभाव व्यापक रूप में तथा अधिक आसानी के साथ अनेकानेक लोगों में फैल सकता है और ऐसी चीज अभिव्यक्त कर सकता है जो उनके आविर्भाव के बिना सम्भव नहीं होती।
अब इसमें समस्या क्या होती है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ स्पष्ट रूप से तो नहीं है परन्तु निहित अवश्य है। उदाहरण के लिए हम किसी साधना के आदर्श, भगवान् श्रीराम या श्रीकृष्ण की भक्ति के आदर्श आदि को लेकर चलते हैं और जब हम थोड़ा अपने भीतर जाते हैं तब हमें आत्मा की क्रिया द्वारा समझ में आ जाता है कि हमें जीवन में अमुक आदर्श की दिशा में प्रयास करना चाहिये। और हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तब उस आदर्श को चरितार्थ करने हेतु हमारे अंदर संकल्पशक्ति जागृत होती है और हम उसे आत्मसात् करने तथा उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ अवतार की उपस्थिति से दो काम होते हैं। एक तो यह कि अपने अन्दर से किसी आदर्श या किसी उद्देश्य की ओर आकृष्ट होने पर भी अपनी इच्छा-शक्ति को एकत्र कर के उस दिशा में लगाना मनुष्य के लिए आसान नहीं होता। मनुष्य प्रपंचों में इतना फँसा होता है कि यदि उसे बुद्धि से यह समझ में आ भी जाए कि बिना भगवान् के जीवन बेकार है तो भी भगवान् की ओर अपनी इच्छा-शक्ति को लगाना इतना आसान नहीं होता। और वह लगाए बिना प्रत्युत्तर बहुत ही थोड़ी मात्रा में मिलता है। इस समस्या के समाधान के लिये अवतार की आवश्यकता होती है। आवश्यक नहीं है कि अपनी बाह्य प्रकृति में अवतार को इस पूरी प्रक्रिया का पता हो परंतु अंतर में उसे यह महसूस हो जाता है कि कहाँ-कहाँ क्या-क्या होना है। क्योंकि अवतार उस केन्द्रीय संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ सभी जीवों के संकल्प जुड़े हुए हैं और यहीं से उनको प्रत्युत्तर आता है। अब अवतार चाहे तो वह किसी भी व्यक्ति के भीतर से संकल्प आये बिना ही उसके लिए स्वयं ही संकल्प कर सकता है और उसका प्रत्युत्तर उस व्यक्ति को उसी प्रकार प्राप्त होगा मानो यह उस व्यक्ति के स्वयं के ही संकल्प का प्रत्युत्तर हो। श्रीमाँ का संकल्प उसी प्रकार उत्तर देगा मानो व्यक्ति ने स्वयं अभीप्सा कर के, बहुत साधना कर के अपना सब कुछ अर्पित कर के स्वयं यह संकल्प किया हो, और उसी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में वे चीजें अभिव्यक्त होने लग जाती हैं। यह एक बात हुई। इसके अलावा एक तत्त्व और है जो कि नये अवतार के आविर्भाव को अनिवार्य बना देता है और उसके बिना काम चल ही नहीं सकता।
स्वयं श्रीमाँ और श्रीअरविन्द का उदाहरण तो हमारे सामने ही है। यदि हम साधना करते हैं और भगवान् राम से, कृष्ण से जुड़े हुए भी हैं, उनसे हमें सहायता भी प्राप्त है, उनकी उपस्थिति भी ठोस रूप से विद्यमान है तो वे हमारे भीतर उस संकल्प को जगा देते हैं जो पूरी तरह नहीं तो भी कुछ हद तक हमें साधना में तो लगा ही देता है। यह काम तो अभी भी हो रहा है और होता ही है। परन्तु इसमें एक बहुत बड़ी सीमितता है। वे जो अभीप्सा हममें जगाते हैं उसके आधार पर हम स्वयं जितनी भी मेहनत करें पर अपने संसाधनों के आधार पर हम एक परिधि से बाहर नहीं जा सकते। हमारी अभीप्सा उस अमुक अवतार द्वारा जो कुछ भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व में अभिव्यक्त किया था उसी तरफ जाएगी और उससे सीमित होगी। उसके परे नहीं जा सकती। क्योंकि हमारी तो परमात्मा से सीधे सम्पर्क की कोई व्यक्तिगत क्षमता है नहीं। अब श्रीमाँ और श्रीअरविन्द के आने के बाद हमें यह लाभ हुआ कि वे हमारी अभीप्सा को सक्रिय तो कर ही रहे हैं, जो कि पहले भी हो रही थी, परन्तु इसके अतिरिक्त वे परमात्मा के व्यक्तित्व की ऐसी चीजें हमारे सामने ले आए हैं जो पहले सचेतन रूप से नहीं थीं। साथ ही वे हमारे संकल्प को उन नये पहलुओं के प्रति भी जागृत कर रहे हैं जिनके प्रति हम पहले जागृत नहीं हो सकते थे। जिनमें क्षमताएँ होतीं वे भी एक सीमा से अधिक आगे नहीं जा सकते थे। परन्तु परमात्मा के व्यक्तित्व की यह जो नयी अभिव्यक्ति होती है वह पहले की अभिव्यक्तियों को अतिक्रम कर जाती
है। भगवान् श्रीराम ने जो अभिव्यक्त किया, श्रीकृष्ण उसे अतिक्रम कर गये। श्रीराम और श्रीकृष्ण ने जो अभिव्यक्त किया उसे श्रीमाँ व श्रीअरविन्द की नवीन अभिव्यक्ति ने अतिक्रम कर दिया। इस नए तत्त्व की तो हम स्वयं अभीप्सा कर ही नहीं सकते थे। और यदि इस नए तत्त्व की अभिव्यक्ति धरती पर नहीं आए तो फिर समृद्धता कैसे आएगी, नए आयाम कैसे खुलेंगे? भगवान् की ज्यों-ज्यों उत्तरोत्तर विकसनशील अभिव्यक्ति होगी त्यों ही त्यों प्रकृति में अधिक समृद्धता आती जाएगी। इसलिए अवतार न केवल उन व्यक्तियों के संकल्प को जागृत ही कर देते हैं अपितु उसे उस दिशा में सक्रिय बना देते हैं, उस ओर उद्घाटित कर देते हैं जिसकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार यह दोहरी क्रिया हो गई। और अवतार का यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव है। अन्यथा यदि केवल संकल्प करने की ही बात होती तो नवीन अवतारों की आवश्यकता ही नहीं होती।
साथ ही, यह जो नया प्रकटन आता है पृथ्वी पर उसकी अभिव्यक्ति में तथा उसकी स्थापना में समय इसलिए लगता है क्योंकि शुरू में हर कोई इतना तैयार नहीं होता कि उस नए प्रकटन को ग्रहण कर सके। इसके लिए उस तत्त्व तक जाकर एक सेतु बनाना और उनकी शिक्षा का विस्तार करना आवश्यक होता है ताकि लोग उस नये पहलु के प्रति अभीप्सा कर अपने मन, प्राण को तैयार कर सकें। अन्यथा व्यक्ति आगे जा ही नहीं सकता था। यह परमात्मा का अधिक पूर्ण प्रकटन है और इसके ये दो पहलू हैं। एक तो यह कि जो लोग इस स्तर तक नहीं आ पाते कि वे भगवान् की ओर सचेतन रूप से चल पाते, वे भी उसके प्रभाव से उस ओर चल पड़ते हैं। और वे भी भगवान् की उस अभिव्यक्ति की ओर चल पड़ते हैं जो अन्यथा चल ही नहीं पाते। भगवान् के नवीन पक्ष को भगवान् स्वयं ही तो प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि सारे बन्दर मिल कर कितना भी प्रयास कर लें तो भी मानव नहीं बन सकते, मानव ही बन्दर को नई चीज बता सकता है। अतः परमात्मा की नयी अभिव्यक्ति से ही ये नए तत्त्व सक्रिय हो सकते हैं।
यहाँ यह स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया गया है परन्तु जो श्रीअरविन्द बता रहे हैं उसके अनुसार यह तर्कसम्मत है कि ये दोनों चीजें इसमें निहित हैं। केन्द्रीय चीज तो श्रीमाताजी ने बता ही दी। अवतार की जहाँ तक आवश्यकता है तो उसमें ये दोनों बातें हैं। नया अवतार नयी अभिव्यक्ति के लिये आता है। इसलिये श्रीमाताजी और श्रीअरविन्द का आना आवश्यक था। वे अतिमानस को अभिव्यक्त करने के लिये आए थे। परमात्मा की एक नयी कला को अभिव्यक्त करने के लिये नए अवतार का आना आवश्यक होता है।
इस पूरे विषय पर इतनी चर्चा हम इसी कारण कर पा रहें है क्योंकि श्रीमाँ व श्रीअरविन्द का आविर्भाव हुआ अन्यथा तो इन बातों की कल्पना तक भी नहीं हो सकती थी। उनके आगमन से मनुष्यजाति के समक्ष एक बहुत बड़ा अध्याय खुल गया है। इतना विशाल काम हुआ है जैसा पहले कभी हुआ ही नहीं। और वे अपना काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, उसे अवश्य पूरा करेंगे। जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ या संकटावस्थाएँ हम वर्तमान में देखते हैं वे तो ऐसी चीजें हैं जो परमात्मा की अनंत संभावनाओं में निहित थीं और जिनकी यदि अभिव्यक्ति न हुई होती तो परमात्मा की ये सारी संभावनाएँ सामने नहीं आतीं। अतः इस दृष्टिकोण से ये विशेष परिस्थितियाँ हैं। सारी अभिव्यक्तियाँ परमात्मा की अनंत संभावनाओं को बाहर लाने के साधन का काम करती हैं।
संदर्भ सूची
इस पुस्तक में गीता के श्लोकों पर प्रस्तुत की गई टीका श्रीअरविन्द व श्रीमाँ की कृतियों से ली गई है। जिन श्लोकों के लिए टीका दी गई है, उनकी श्लोक संख्याओं के सामने उन टीकाओं के संदर्भ दिये गये हैं। प्रस्तावना व परिशिष्ट में उद्धरण जिस पुस्तक से लिये गये हैं उनकी खण्ड संख्या तथा पृष्ठ संख्या दी गई है। (S) का अर्थ है The Synthesis of Yoga (CWSA 23- 24), (L) का अर्थ है Letters on Yoga (CWSA 28-31), (Svt.) का अर्थ है Savitri (CWSA 33-34), जहाँ संदर्भों के लिए खण्ड संख्या नहीं दी गई है वे सभी उद्धरण Essays on the Gita (CWSA 19) से लिए गए हैं। श्रीअरविन्द की अन्य पुस्तकों के संदर्भों के लिए खण्ड संख्या तथा पृष्ठ संख्या (CWSA vol no : page no.) दी गई है। श्रीमाँ की कृतियों से लिए गए उद्धरणों के लिए खण्ड संख्या तथा पृष्ठ संख्या (CWM Vol no : page no.) दी गई है।
चूँकि यहाँ मुद्रित उद्धरणों का तथा श्लोकों का अनुवाद अनुवादक द्वारा ही किया गया है अथवा अन्य स्थानों पर मूल विचार को अधिक सुगम, स्पष्ट व सटीक बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध अनुवाद में संशोधन व परिवर्तन किए गए हैं इसलिए उद्धरणों के लिए मूल स्रोतों की ही सूची दी गई है।
प्रस्तावना
I: 4-9, 562-63, 11
II: 29-33, 35-38
अध्याय एक
:12 36:24
23:23 39:S331-333
28:23 47:39-40, 47-48, 45-46, 45,
29:23-24 48-49, Svt.657
32:24
पादटीका (Footnote)
1:20-21
2: Svt.424-25
-------------------------------
CWSA: Complete Works of Sri Aurobindo
CWM: Collected Works of The Mother
अध्याय दो
1:57 45:87
3:57-60 46:87-89
6:25-26 47:S222-23
9:60 48:S96
10:60-61 50:CWSA (13)119, 103
13:61 51:103
14;62 53:92-93
15:61-62 54:102
28:63 55:101-02
30:63-64 58:98-99
31:65 59:99-100
37:66 60:100
38:66, 451-52, 66-67 61:100-01
II: 68 65:101
39:81, 68-80, 94 67:98
III:94 69:214
40:94-95 72:104
41:95-96
पादटीका
1:72-74
2:S683-84
3:S689-90
4:102
5:92
अध्याय तीन
I:105-06
2:106
3:106
4:106-07
5:107-08
6:108
7:108-09
8:109-11
9:111-13
18:115-19
19:115
II 134, 256-57, 135
26:136-37, S272, 139, 141-44 140
III -212-13, L514-15, S95-96. 214
27:231,224-226
28:226-28
29:225,214
33:217,212, 218
35:218
37:S656-57
40:S656
41:99, CWM(5)212-13
42:96-98
43 / S * vt * 0.315 - 16 ,S658-659
पादटीका
1:108
2:109
3:110
4:L433-34
5:S272-273
6:CWSA (21)58
7:S269-70
8:S270
9:S270
10:L(iv)266
11:CWM(3)117
अध्याय चार
3:145 22:181-84
4:146 23:200, 187, S101-05
6:155-56, 159, 156-57 III:S106, 124-28, 114, 119-20
8:147-50, 148, 159-65 24:120-21
9:168-71,174-75 25:121
10:175-76 27:121
11:176 30:121-22
12:147 31:122
13:512-13,6-7 32:122
14:147 35:122-23
II:177 IV:200
17:177-78 37:201
18:178-79 38:204,203-04
20:179-80, 184 40:204-05
21:180-81 42:205
पादटीका
1:150-152
2:L472
3:L476-78 4.CWSA(2), 534-35,537
5:L485-486
6:Svt.67
7:CWM(13)75-76
8:CWSA(2)612
9:Svt.339
10:CWM(8)74-75
11:119-120
12:L(i)89, L(i)92-93
13:S115-16
अध्याय पाँच
1:82 20:188, 189-93, 195-97, 206- 07, 197-98, 208-10
1:82-83
4:83 II:234-36
6:185, 201 23:236
7:83 24:236
9:186 26:237-38
12:S247 28:238-39
15:201-02 29:239-40
पादटीका
1:83-84 2:186
3:202
अध्याय छः
2:240
3:240
6:218-19
9:S698-99, S223, S224-25,
S226-28
10:241
15:242-43
16:CWM(6)428-29
17:243-44
22:242
23:242, S244-45
28:242-43
29:255-56,244
30:244-45
31:245-46, 210-11
32:245-46
35:CWM(4)334-35
36:S72
46:246
47:246, 248-55, 256-58
पादटीका
1: L442
2:368-369
3-CWM(4)336-337
अध्याय सात
1:247-48, 263, 265-66
2:266
3:266
5:266-68, 267-69,270
6:269, 270-71
7:271-72
10:273-74
11:274-75
12:274, 275-76
13:276
14:276-77
II:278-79
15:280-82, 284
16:284-85
18:S550-51
19:S371-72, 315-16
20:285, S159
22:286-87, CWSA(12)88-89
23:286
28:282-83, 287-88, 290
29:290-91
30:291
पादटीका
1:263-64
2:Svt.295
3:267
4:269-70
5:272-73
7:589
8:316
9:287
10:S675
श्रीअरविन्द गीता
श्रीअरविन्द गीता के संदेश को उस महान् आध्यात्मिक गति का आधार मानते हैं जो मानवजाति को अधिकाधिक उसकी मुक्ति की ओर, अर्थात् मिथ्यात्व और अज्ञान से निकलकर सत्य की ओर ले गई है, और आगे भी ले जाएगी।
अपने प्रथम प्राकट्य के समय से ही गीता का अतिविशाल आध्यात्मिक प्रभाव रहा है; परंतु जो नवीन व्याख्या श्रीअरविन्द ने उसे प्रदान की है, उसके साथ ही उसकी प्रभावशालिता अत्यधिक बढ़ गई है और निर्णायक बन गई है।
- श्रीमाँ