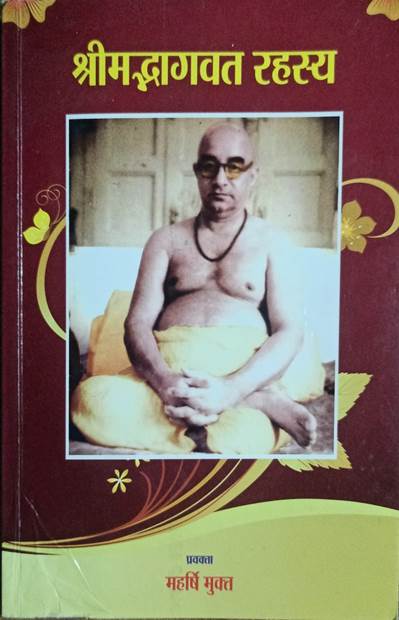
श्रीमद्भागवत रहस्य
महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारसमिति
आत्मवित् शोकं तरतिं
महर्षि मुक्त
श्रीमद्भागवत रहस्य
प्रणेता : महर्षि मुक्त
प्रकाशक : महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचार समिति
केन्द्र दुर्ग (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक 2093/94,
रायपुर (सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशकाधीन)
फोटोटाईप सेटिंग : नेचर ग्राफिक्स शांति चौक, पुरानी बस्ती,
रायपुर (छ.ग.) मो.: 93022-30478
मुद्रक महावीर : आफसेट गीता नगर, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
मो.: 93036-08080
संस्करण : द्वितीय
प्रति : 1000 (एक हजार)
दिनांक : 19 जुलाई 2016
पुस्तक मिलने का पता- डॉ. सत्यानंद त्रिपाठी 61/152, बंधवापारा,
रायपुर (छ.ग.) मो.: 99261-30014
प्रकाशन क्रमांक : 3
मूल्य : 150/-
श्रीमद्भागवत रहस्य
आख्यान सूची क्रमांक
भूमिका, महिमा एवं चतु:श्लोकी भागवत
गजेन्द्रोपाख्यान के माध्यम से अस्तित्व निरुपण श्री कृष्ण जन्मकथा
भगवान कृष्ण की बाललीला, ब्रह्मस्तुति, चीरहरण, उद्वव गोपी संवार, भ्रमर गीत
यदुवंशियों को ऋृषियों का शाप, भगवान कृष्ण का उद्वव को उपदेश हंसोपाख्यान
आरती
आरती सद्गुरुदेव नमामी । पार ब्रह्म-प्रभु अन्तर्यामी ।।
अगुण अपार अलख अविनाशी। अचल विमल प्रभु सब उरवासी ।।
निर्गुण निर्विकार सुखरासी । एक अरूप अलेख अनामी ।। 1 ।।
महिमा नेति नेति श्रुति गावें । नित्य निरंजन सब बतलावें ।।
शेष शारदा पार न पावें । जय सच्चिदानंद अभिरामी ।। 211
वचन किरण तम मोह विनाशक । ज्ञान सूर्य माया के शासक ।।
दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक । ब्रह्मादिक सुर सेव्य नमामी ।। 3 ।।
जब तक कृपा न तुम प्रभु करते। विधि हरिहर क्या भव से तरते ।।
असविचारि गुरु भक्ति जो करते। मिलते राम उन्हें सुखधामी ।। 4 ।।
गुरूवर चरण कमल की छाया। करती दूर ताप त्रय माया ।।
जब तक पूर्ण न होवे दाया। मिलत नहीं शिव अन्तर्यामी ।। 5 ।।
भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के। रूप सकल इंद्रिय संयम के ।।
भूषण शम दम पंच सुयम के । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मम स्वामी ।। 6 ।।
जीवन धन मंजुल निज जन के। अंकुश मद मतंग जन मन के ।।
शुचि पथ परमारथ पथिकन के। इक रस आनंद रूप नमामी ।। 7 ।।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
।। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय ।।
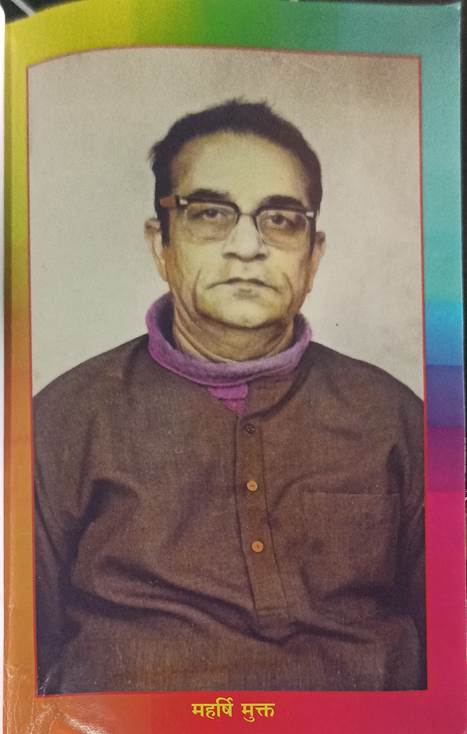
श्रीमद्भागवत रहस्य
महर्षि मुक्त द्वारा श्रीमद्भागवत परमहंस संहिता के साक्षित्व में सप्तदिवसीय अध्यात्म निरूपण दिनांक 8 फरवरी 1969 से 24 फरवरी 1969 तक स्थान- झंडापुर, पोस्ट-बिहार, तहसील-कुंडा, जिला-प्रतापगढ़ (उ.प्र.) पर आधारित यह अनुपमेय और विलक्षण कृति महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचार समिति की अन्यतम उपलब्धि है।
भागवत का अर्थ होता है-भगवान। चूँकि इसमें भागवत के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है, इसलिए प्रस्तुत साहित्य को श्रीमद् भागवत रहस्य नाम से अलंकृत किया गया है। भगवान के चार रहस्य हैं
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुण कर्मकः ।
तथैव तत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् ।।
यावानहं (मैं जैसा हूँ) - भगवान। मैं जैसा हूँ का भाव, मैं जैसा हूँ का रूप, मैं जैसा हूँ का गुण और मैं जैसा हूँ का कर्म। ये चार रहस्य-भगवान-के। इन रहस्यों को उजागर करना सिवाय संतों के अन्य किसी विद्वान या साधु संन्यासी के वश की बात नहीं है। इन रहस्यों का सम्यक् रूप से अपरोक्ष अनुभूति इस पुस्तक का प्राण है, इसलिए यह चेतन साहित्य है।
चतुःश्लोकी भागवत के माध्यम से इस तरह का निरुपण पहले कभी ना हुआ है और ना ही आगे होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान नारद एवं राजा प्राचीनबर्हि संवाद पुरञ्जनोपाख्यान, गजेन्द्रोपाख्यान, ब्रह्मा स्तुति, उद्धव गोपी संवाद, हंसोपाख्यान आदि प्रसंगों के माध्यम से जीव-ईश्वर की एकता, कर्म, उपासना, ज्ञान, भक्ति, मन-माया-जगत आदि का चारों प्रमाणों से संसिद्ध निरुपण की अलौकिक छटा देखते ही बनती है जो कि कहीं और देखने-सुनने में नहीं आता। निरुपण शैली की सहजता एवं अकाट्य प्रमाणों से वेदान्त जैसे क्लिष्ट विषय भी जनसाधारण को हृदयंगम हो जाता है। यह प्रवक्ता का तपोबल एवं संयम है। यह एक चमत्कार है।
मैं इस सांगोपांग अनुपम कृति के प्रवक्ता महर्षि मुक्त के संबंध में इतना ही कहूँगा कि- 'आप प्रकट भये विधि न बनाये।' ये अनिकेत अवधूत थे। किसी पंथ, सम्प्रदाय से सर्वथा निर्लिप्त। अविरल रूप से सत्य के सार्वभौम प्रचारक महर्षि मुक्त की साधना-तपस्या का साक्षी, इनका साहित्य ही है, जीवन पर्यन्त, भेद बुद्धि का त्याग करके सत्य का ही प्रचार-प्रसार किये। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धारणा को धारण करके अपने लिये एक घास-फूस की कुटिया भी नहीं बनाई उन्होंने।
वे कहा करते थे कि फकीरी हमारी जागीर है और हमेशा हमारी मुट्ठी में है। इनका विश्वास था कि पंथ, सम्प्रदाय में आने से व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाती है और वह अध्यात्म से कोसों दूर हो जाता है।
आज भी इनके लाखों की संख्या में समर्पित अनुयायी हैं लेकिन सभी पंथ, सम्प्रदाय से अलग-थलग एकदम स्वतंत्र ।
इनकी कृतियों में मुक्तानुभव भजन माला, भजन मुक्त लहरी, मुक्त दोहावली, मुक्तोद्गार, पैगाम-ए-मुक्त आदि मौलिक रचनायें हैं। इन सभी रचनाओं में महर्षि मुक्त सूत्रावली अनुपम एवं अद्वितीय कृति है। इसमें उपनिषद्, श्रीमद्भागवत परमहंस संहिता, श्रीमद्भागवत गीता एवं रामायण के तत्वपरक आध्यात्मिक प्रसंगों की रचना की गई है, जिनकी संख्या लगभग पच्चीस हजार के करीब होगी जो विश्व मानव के लिए अनुपम धरोहर है। इन्हें प्रकाशित कराकर आप तक पहुँचाने का प्रयास जारी है।
श्रीमद्भागवत रहस्य का द्वितीय संस्करण आपको सौंपते हुए हमें अपार प्रसन्नता है। प्रकाशन में विलम्ब के लिए हमें खेद है। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में चौथे दिन के द्वितीय प्रहर की कथा कृष्ण जन्म का अंश अप्राप्त होने के कारण छूट गया था किन्तु अब वह प्राप्त हो गया है और उसे जोड़ दिया गया है जिससे पुस्तक की कमी पूरी होकर अब एक सांगोपांग कृति बन चुकी है।
प्रथम संस्करण में जिन महानुभावों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यज्ञ रुप से सहयोग मिला है, उनकी लगन, श्रम और सहयोग स्तुत्य है। यह उन्हीं के भगीरथ प्रयास का सुफल है कि देव दुर्लभ सदुपदेश से परिपूर्ण कृति हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं। वे सभी महानुभाव साधुवाद के पात्र हैं। समिति उनकी आभारी है।
द्वितीय संस्करण के संशोधन में श्री रूपेन्द्रनाथ तिवारी जी, एम.ए. (दर्शनशास्त्र, हिन्दी) का सहयोग अत्यंत प्रशंसनीय एवं सराहनीय रहा है। समिति के संरक्षक डॉ. सत्यानंदजी महाराज, जिनकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद स्वरुप इस श्रम साध्य कार्य को हम साकार कर सके, समिति उनका चिर आभारी है।
नेचर ग्राफिक्स के संचालक भाई नितिन कुमार झा जी जिन्होंने ऐसे कठिन साहित्य को बड़ी लगन एवं सावधानीपूर्वक टंकण करके इसकी भाषा को शुद्ध एवं सुवाच्य बनाया है वे साधुवाद के पात्र हैं। हम उनके आभारी हैं।
हमारा पूरा-पूरा प्रयास रहा है कि कृति के प्रकाशन में त्रुटि अथवा अशुद्धि न रह जाये फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। समिति के इस प्रयास को विद्वतजन सराहेंगे और भक्त साधुजन मान्यता देंगे एवं जिज्ञासुगण अवगाहन करेंगे इन्हीं आशाओं के साथ, अलं !
आपका अभिन्न
(डॉ. प्रीतम मिश्रा)
अध्यक्ष
महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति
केन्द्र-दुर्ग (छ.ग.)
स्थान : रायपुर
दिनांक : 19 जुलाई 2016 आषाढ़, गुरु पूर्णिमा
_________________________________________________________________________________
।। श्री गणेशायनमः ।।
।। श्री गुरुवेनमः ।।
नारायणोपनिषत्
ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति । गुनारायणात् प्राणो जायते। मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणाद् ब्रह्मा जायते। नारायणात् रुद्रो जायते। नारायणाद् इन्द्रो जायते । नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते ।
नारायणाद्वादशादित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते । नारायणात्प्रवर्तन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते ।
अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः। शक्रश्च नारायणः। कालश्च नारायणः । दिशश्च नारायणः । विदिशश्च नारायणः। ऊर्ध्वं च नारायणः । अधश्च नारायणः। अन्तर्बहिश्च नारायणः।
नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् । निष्कलंको निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति।
ॐ शांतिः ! शांतिः !! शांतिः !!!
प्रथम दिवस
भूमिका, महिमा एवं चतु:श्लोकी भागवत
18-2-1969, प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
अनन्त नाम रूपों में अभिव्यक्त, अहमत्वेन प्रस्फुरित, महामहिम, स्वात्मस्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित आत्मजिज्ञासुगण !
'उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्यवरान्निबोधत ।'
(कठो.उ.)
अनादिकाल से अविद्या के घोर अंधकार में सोने वालों भव्य जीवो। 'उत्तिष्ठत'-उठो । स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो। किसी श्रेष्ठ महापुरुष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण होकर अपना आत्म-कल्याण करो।
अनन्त जन्मों के पूर्वार्जित पुण्यों के उदय होने पर आज से यहाँ पर श्रीमद् भागवत, महापुराण परमहंस संहिता के आधार पर अध्यात्म निरूपण होने जा रहा है। जिस प्रकार मंदिरों में किसी मूर्ति की अध्यक्षता में भगवान की आराधना होती है उसी प्रकार श्रीमद् भागवत, उपनिषत, श्रीमद्भगवत गीता, श्री रामायण आदि शास्त्रों की अध्यक्षता में, उनके साक्षित्व में, सिद्धांतों द्वारा अध्यात्म निरूपण होता है।
आत्मजिज्ञासुओं ! आज इस पावन बेला में जो कुछ अध्यात्म निरूपण होगा वह सब श्रीमद्भागवत परमहंस संहिता के साक्षित्व में होगा। भागवत पुराण के माध्यम से होगा अर्थात् जो कुछ भी यहाँ कहा जायेगा उसे श्रीमद् भागवत पुराण समर्थन करेगा। इस पुराण की अलौकिक महिमा है। एक जन्म नहीं अनन्त जन्मों के जब पुण्य होते हैं तभी श्रीमद् भागवत पुराण अध्यात्म तत्व श्रवण करने का अवसर आता है। इसमें स्वस्वरूप स्थित श्री परमहंस स्वामी शुकदेव जी राजा परीक्षित की आत्म तत्व का दर्शन कराते हैं। इस पुराण में अनेक वेद मंत्रों सहित उनके तत्वों की सुंदर-सुंदर कथा, आख्यानों द्वारा प्रतिपादन एवं उपदेश हुआ है।
स एवेद्ꣲ᳭ सर्वम् । नारायणेवेद्ꣲ᳭ सर्वम् । आत्मैवेद् सर्वम् ।ꣲ᳭ अहमेवेद् सर्वम। वासुदेवः सर्वमिति इत्यादि मंत्रों का उपदेश श्री स्वामी शुकदेव जी राजा परीक्षित को किए हैं।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराष्ट्
तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा,
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ।।
(श्रीमद्भागवत 1/1/1)
धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् ।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीस्वरः
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रुषुभिस्तत्क्षणात् ।।
(श्रीमद्भागवत 1/1/2)
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् ।
पिवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ।।
(श्रीमद्भागवत 1/1/3)
ये तीनों श्लोक श्रवण, मनन, निदिध्यासन के रूप में महर्षि व्यास जी प्रतिपादित किए गये हैं।
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।।
(वृहदा 4-5-6)
श्री भगवान व्यास जी श्रुति के इसी मंत्र को छंद के रूप में छंदबद्ध कर दिये हैं। यह आत्मा द्रष्टव्यः (देखने योग्य) अनुभव करने योग्य, श्रोतव्य:' सुनने योग्य एवं निदिध्यासितव्यः- निदिध्यासन करने योग्य है इसीलिए इस आत्म तत्व का विवेचन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सामीप्य में ग्रहण करना चाहिए।
हाँ जी-श्रवण, मनन, निदिध्यासन का इन श्लोकों में निरूपण हुआ है। तो इनका स्वरूप क्या है? देखो किसी भी मंत्र को समुचित ज्ञान के लिए मंत्र समझने के लिए, मंत्र को तीन तरह से परखना चाहिए। अर्थानुसंधान द्वारा भावानुसंधान द्वारा और लक्ष्यानुसंधान द्वारा। वृत्ति कहो या मन कहो ये दोनों परस्पर एक ही भाव के द्योतक हैं। संत समाज में इसी को 'सुरति' कहते हैं । साधारण भाव में मन कहते हैं। देखो समझो विषय (डंडे का उदाहरण देकर विषय समझते हैं।) डंडे का जो आकार है यह हुआ डंडे का अर्थ और इसमें जो वृत्ति की एकाग्रता, उसे कहते हैं अर्थानुसंधान। लकड़ी जो है वह डंडे का भाव है। इसमें जो वृत्ति की एकाग्रता, उसे कहते हैं भावानुसंधान और इसका लक्ष्य क्या है? चेतन तत्व भगवान आत्मा। इसमें जब वृत्ति एकाग्र हो जाय तो उसे कहते हैं लक्ष्यानुसंधान ।
श्रवणं शतगुणं विद्यान्मननं मननादपि ।
निदिध्यासं लक्षगुणमनन्तं निर्विकल्पकम् ।।
(विवेक चूड़ामणि ल.नि. 365)
श्रवण की अपेक्षा मनन करने में सौ गुना अधिक फल होता है। मनन की अपेक्षा निदिध्यासन करने में एक लाख गुना फल होता है। निदिध्यासन की अपेक्षा चित्त का निर्विकल्प हो जाना-इसका फल अनन्त गुना होता है।
धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां ।
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् ।।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ।।2।।
यह मनन है।
निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् ।
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ।।3।।
यह निदिध्यासन है।
देखो-बालक श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता के गले में सर्प डालने के अपराध में राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज के सातवें दिन तक्षक जाति का सर्प आकर तुझे डस लेगा। राजा परीक्षित राज्य एवं प्राण का मोह त्याग कर उत्तराभिमुख हो (उत्तर दिशा की ओर मुँह करके) व्याकुल दशा में बैठ गया और उसे यह निश्चय हो गया कि आज के सातवें दिन अवश्यमेव मृत्यु हो जायेगी। इसी कारण उसके हृदय में पूर्ण वैराग्य जाग्रत हो गया। मछली की तड़प की नाई उसका मन आत्म तत्व को जानने के लिए उत्कंठित हो गया कि मेरा आत्म कल्याण कैसे हो? और यह भी सात ही दिन में। कारण? अब उसे सात ही दिन जीना है।
अत्रिर्वसिष्ठश्च्यवनः शरद्वानरिष्टनेमिभृगुरङ्किराश्च ।
पराशरौ गाधिसुतोऽथ राम उतध्य इंद्रप्रमदेध्मवाहौ ।।
मेधातिथिर्देबल आष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्लादः ।
मैत्रेय और्वः कवषः कुम्भयोनिद्वैपायनो भगवान्नारदश्च ।
अन्ये च देवर्षिब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च ।
नानार्षेयप्रवरान्समेतानभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे ।।
(श्रीमद् भागवत 1/19/9-10-11)
उस समय बड़े-बड़े देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षियों का शुभागमन, जहाँ राजा परीक्षित बैठे थे हुआ। यह निर्विवाद सिद्धांत है, यह ईश्वरीय विधान है कि जिस समय आत्म जिज्ञासु को मछली के समान तड़प यानी आत्म जिज्ञासा जागृत होती है अर्थात् उसे आत्मतत्व जानने की व्याकुलता होती है, उसका चित्त जब संसार से पूर्णतया उपराम हो जाता है तब महापुरुषों का दर्शन स्वयमेव होता है। स्वयं वे दर्शन देंगे, उसका कल्याण करने हेतु आ जाते हैं और इस तरह का समागम संसार से तरने का नोटिस है। श्रीमद् भागवत के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्द्ध में महाराजा मुचकुंद जी भगवान की स्तुति करते हैं-
भवापवर्गोभ्रमतो सदा भवेज्जनस्य तहांत्त्युत सत्समागमः ।
सत्सङ्गगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावेरेरो त्वयि जायते मतिः ।।
(श्रीमद् भागवत 10/51/54)
हे अच्युत ! हे प्रभो ! भगवान ! जब जीवों के अपवर्ग अर्थात् मोक्ष होने को होता है, जब आप संसार से उनके उद्धार की इच्छा करते हैं तो अपने भागवत (संतों) का दर्शन, उनका समागम उन्हें आप स्वयं ही करा देते हैं। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष होता है।
अ का अर्थ हुआ नहीं, प वर्ग का अर्थ हुआ प फ ब भ म ।
जानते ही हो व्याकरण में क वर्ग अर्थात् क ख ग घ ङ
च वर्ग अर्थात् च छ ज झ ञ इसी तरह प वर्ग का अर्थ हुआ प फ ब भ म ।
हाँ जी, प का अर्थ पापं नास्ति। जब पाप नहीं तो फिर पुण्य भी नहीं। पुण्य पाप दोनों गए। पुण्यं पापं नास्ति ।
फ का अर्थ फलं नास्ति। फल की आकांक्षा नहीं।
व का अर्थ बंधनं नास्ति। जब फल की आकांक्षा नहीं तो फिर बंधन कैसे? किए कर्मफल कहाँ।
भ का अर्थ - भयं नास्ति। कर्म फल ही तो बंधन का कारण है, जिससे सुख-दुःख मिलता है। जब बंधन ही नहीं तो भय किसका ।
म का अर्थ- मानं नास्ति। मान नहीं। जब मान नहीं तो अपमान भी नहीं। तो जहाँ प वर्ग न हो उसे कहते हैं अपवर्ग।
अरे भाई ! बंधन के ही अंदर मान-अपमान है। जहाँ पुण्य पाप नहीं वहाँ उसका फल क्या होगा और जब फल ही नहीं तो बंधन किसका होगा? और जब बंधन नहीं तो फिर भय किसका। इसी को कहते हैं अपवर्ग अर्थात् मोक्ष। जिस समय किसी को अतीव आत्म जिज्ञासा, आत्म कल्याण की भूख प्रज्ज्वलित हो जाती है तो सर्वप्रथम संतों का दर्शन होता है और संत समागन से उसका मोक्ष हो जाता है।
जिस समय राजा परीक्षित अपने आत्म कल्याण की भावना में ध्यान मग्न था उसी समय ध्यान टूटते ही देखता है कि झुण्ड के झुण्ड महात्मागण आ रहे हैं, जिससे कि राजा परीक्षित का आत्म कल्याण हो। महात्मागण जब राजा परीक्षित के पास आ गए तब राजा उठा और उन सबको अभिवादन, दण्ड का प्रणाम किया तथा सबका पूजन किया और सबके सन्मुख हो प्रार्थना किया का राजा निवेदन करता है कि हे प्रभो! मेरा जीवन सात ही दिन शेष है। थोड़ा का समय है। इस थोड़े समय में मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा? मुझसे अज्ञानतावश अनिष्ट हो चुका है। पंच वर्षीय बालक श्रृंगी ऋषि के श्राप से आज से सातवें दिन तक्षक जाति का सर्प आकर मुझे डस लेगा। मेरी मृत्यु तो सामने खड़ी है। कि मुझे उपदेश करिये जिससे कि मेरा आत्म कल्याण हो।
राजा परीक्षित ने अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा भगवान व्यास, वामदेव, जा वसिष्ठ महर्षिगणों के समक्ष रखी, परन्तु उस समय ऋषियों को कोई उपायको नहीं सूझा। किसी की बुद्धि काम नहीं आई। उसी समय सोलह वर्षीय व्यासनंदन श्री शुकदेव स्वामी दिगम्बर रूप में, अवधूत वेश में, श्याम रंग, प्रकीर्ण जटाएँ,ग लम्बी-लम्बी भुजाएँ आजानुबाहु निजानंद में मस्त स्वरूप आत्मा में लीन, मुस्कराते हुए उस सभा में जहाँ ये महर्षिगण बैठे थे, आए। राजा परीक्षित ने यही जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न भगवद्धर्म के परिज्ञाता भगवान वादरायणि स्वामी शुकदेवजी के समक्ष रखा कि हे प्रभो! मेरा उद्धार कैसे हो? मैं आर्त हूँ। आज से सातवें दिन ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डस लेगा। मैं मृत्यु के निकट हूँ। इस दशा में मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा? इस संसार सागर से मेरा उद्धार कैसे होगा? यहीं से श्री स्वामी शुकदेवजी और राजा परीक्षित का संवाद शुरू होता है।
एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा ।
प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणिः ।।
(श्रीमद्भागवत 1/19/40)
इस प्रकार सम्राट परीक्षित की जिज्ञासा देखकर भगवद्धर्म के परिज्ञाता भगवान बादरायणि श्री स्वामी शुकदेवजी बोले-
वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप ।
आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः ।।
(श्रीमद् भागवत 21/1 / 1)
हे राजन! एष ते प्रश्नः वरीयान् । जगत के जीवमात्र के कल्याण के लिए यह तुम्हारा प्रश्न महान श्रेष्ठ एवं आत्म वित्सम्मत है। यानी बड़े से बड़े आत्मवेत्ता पुरुष भी तुम्हारे इस प्रश्न का समर्थन करते हैं। राजा परीक्षित का यह आत्मपरक प्रश्न कि किस तरह संसार सागर से उद्धार हो, जीवमात्र का कल्याण कैसे हो? श्री स्वामी शुकदेवजी के समक्ष रखा गया।
बड़े-बड़े आत्मनैष्ठिक विद्वान महात्माओं के समक्ष यदि कोई प्रश्न करना हो तो यही एकमात्र प्रश्न करना चाहिए कि प्रभो! मैं कौन हूँ? यथार्थ में यह प्रश्न सुंदर एवं मौलिक है। हालांकि यह प्रश्न सूक्ष्म है और जैसी आशा की जाती है कि इसका उत्तर भी छोटा होगा, परन्तु ऐसा नहीं है। उत्तर इतना विस्तृत है कि जीवन पर्यन्त भी इस प्रश्न पर विवेचन हो फिर भी वह अनंत है। इस छोटे से प्रश्न में अनेक सारगर्भित समाधान निहित हैं। इस संदर्भ में एक वृद्धा कुमारी का दृष्टांत सुनो- कैसे एक छोटे से प्रश्न में अनेक समस्याएँ भरी रहती हैं।
किसी समय एक ब्राह्मण कुमारी के शादी योग्य होने पर उसके विवाह हेतु वर ढूँढ़ा गया। दैवयोग-कन्या का अभाग्य, विवाह के पूर्व ही चुना हुआ वर मर गया। तब गाँव के लोग उसके लिए दूसरा उपयुक्त वर ढूँढ़ने लगे, परन्तु अभाग्य कन्या का कि कोई भी ढूँढ़ा गया वर उसे प्राप्त न हुआ। विवाह के पूर्व ही वह मर जाता था। समय बीत गया, वह कुमारी अब कुमारी न रही, चालीस वर्ष की वृद्धा हो गई। अब कौन शादी करे। विवाह न हुआ। एक बार कोई महात्मा उसे उपदेश कर गए कि तू इन्द्रदेव की आराधना कर, तेरे भाग्य फिर सकते हैं। आराधना से इन्द्रदेव प्रसन्न होकर जब वरदान देने के लिए प्रगट होंगे तो उनसे वरदान मांगना कि 'मे पुत्राः स्वर्णपात्रे भुञ्जीरन्।' मेरे पुत्र स्वर्ण पात्र में खीर का भोजन करें।
वह वृद्धा कुमारी श्री इन्द्रदेव की बड़ी भक्ति भाव से आराधना की। कुछ साल बाद उसकी तपस्या फलवती हुई। इन्द्रदेव प्रगट हुए और कहे कि देवि ! वर वृणीश्व-वर मांगो। वह ब्राह्मणी कहती है कि 'मे पुत्राः स्वर्णपात्रे भुञ्जीरन् ।' मेरे पुत्र स्वर्णथाल में भोजन करें और यहाँ यह हाल कि वृद्धा कुमारी के विवाह का ही पता नहीं, फिर पुत्र कहाँ, धन कहाँ। इन्द्रदेव भी चक्कर में पड़े। वृद्धा कुमारी के विवाह का ही पता नहीं, परन्तु सब कुछ मांग लिया। इन्द्रदेव तथास्तु कहकर अन्तर्द्धान हो गए। इन्द्रदेव की कृपा से वृद्धाकुमारी को कौमार्यपन, सुंदर षोडसी रूप मिला। शादी हुई, धनधान्य से सम्पन्न हुई और पुत्र लाभ हुआ क्योंकि वर ही ऐसा मांगा गया था। कहीं कंगाल का पुत्र भी सोने की थाली में भोजन करेगा? इन्द्रदेव को उन्हें सम्पन्न परिवार बनाना पड़ा। तब यह वरदान सत्य हुआ। इसी प्रकार प्रश्न तो छोटा-सा है कि 'मैं कौन हूँ?'
'अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम् ।
पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा ।।
(श्रीमद् भागवत 1/19/37)
श्री चरणों के सान्निध्य में पड़े शिष्य को गुरुओं से यही उपदेश, यही गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि प्रभो! मेरा आत्म कल्याण कैसे हो?
वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप ।
आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः ।।
राजन् ! तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर सारगर्भित एवं मौलिक है। इससे तो तुम्हारा ही नहीं वरन् जीवमात्र का कल्याण होगा। तुम चिंता न करो। तुम्हें तो अभी सात दिन जीना है। वस्तुतः जब आत्मतत्व को जानने की प्रबल इच्छा हो तो सात दिन का भी समय बहुत अधिक है। इसके लिए तो दो घड़ी का ही समय पर्याप्त है और यदि आत्म कल्याण की जिज्ञासा प्रबल नहीं है तो सात दिन क्या एक हजार वर्षों का समय भी अधिक नहीं है। आत्म जिज्ञासा विहीन पुरुषों का उद्यम वैसा ही है जैसे कुत्ते की पूँछ। कुत्ते की पूँछ उसके भी काम की नहीं और उसे काट दो तो हानि भी नहीं। इसी तरह बकरी के गले की निर्दुग्ध स्तन, उससे दूध तो निकलता नहीं व्यर्थ ही लटकता रहता है। आत्म जिज्ञासा के बिना वेदों का अध्ययन भी ऐसा ही प्रयास है। यदि आत्म जिज्ञासा प्रबल है तो दो घड़ी जीवन ही पर्याप्त है। जैसे राजा खट्वांग को जिन्हें दो घड़ी के उपदेश से ही आत्मलाभ हुआ था। वे राजर्षि सूर्यवंश में हुए थे। उनका सारा जीवन ऐश-आराम, आमोद-प्रमोद आदि विषयों में ही बीत गया। जब जीवन सिर्फ दो घड़ी शेष रहा तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान की उत्कट अभिलाषा हुई। श्री भगवान वामदेव की कृपा से राजा को बोध हुआ और वह संसार सागर से तर गया। इससे सिद्ध है कि आत्म कल्याण के जिज्ञासुओं के लिए समय का प्रतिबंध नहीं है। बशर्ते कि आत्म कल्याण की भावना, जिज्ञासा प्रबल हो। राजा परीक्षित की प्रबल जिज्ञासा थी कि मेरा आत्म कल्याण कैसे हो? इसलिए श्री शुकदेव स्वामी के प्रसाद से उसका आत्म कल्याण हुआ।
श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। साथ ही साथ सृष्टि के सृजन का और भगवान के अवतार आदि का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंध के नवें अध्याय में ब्रह्माजी को भगवान नारायण द्वारा ब्रह्मतत्व के उपदेश का वर्णन है जिसे चतुः श्लोकी भागवत कहते हैं। यही परम उपदेश बीज मंत्र है। यह पावन कथा अब प्रेम से सुनो। आत्म जिज्ञासुओं! दोनों समाज प्रकृति एवं पुरुष जो जहाँ बैठे हो ध्यान से सुनो- आनंद लो।
सृष्टि के आदि में श्री शेषशायी भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में श्री ब्रह्माजी हुए। इसी से इनका नाम कमलोद्भव है- कमल से पैदा हुए हैं। श्री ब्रह्माजी ने दृष्टि फैलायी, कमल के चारों तरफ उन्हें सिर्फ जल ही जल दिखा। जल ही जल अपने चारों तरफ देख के कुछ निश्चय न कर सके कि वे कहाँ हैं। उनको जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ? तो वे कमलनाल में चक्कर लगाने लगे, परन्तु वर्षों बीतने पर भी जब वे अपने आधार का पता न लगा सके तो हारकर कमल में बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए? एकाएक उन्हें प्रणव (ॐ) नाद (शब्द) सुनाई पड़ा और 'त', 'प' ये दो अक्षर तीन बार सुनाई पड़ा-तप, तप, तप सुने तो वे कमल में ही आसन जमा हजारों वर्ष तपस्या किए। उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी के समक्ष भगवान नारायण प्रगट हुए। ब्रह्माजी ने स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने ब्रह्माजी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश किया। वस्तुतः इसी चतुःश्लोकी भागवत में भगवान नारायण द्वारा ब्रह्माजी को जो उपदेश हुआ है यही सम्पूर्ण भागवत है। इसी की व्याख्या, उपदेश श्री स्वामी शुकदेवजी राजा परीक्षित को किए हैं। बाद में श्री स्वामी शुकदेवजी के पिता महर्षि व्यासजी ने चतुःश्लोकी भागवत को आधार मानकर श्रीमद् भागवत पुराण बड़े ग्रंथ का निर्माण किया है।
वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कर्तरि ।
परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे ।।
(श्रीमद् भागवत महा. 2/72)
तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुः श्लोकसमन्वितम् ।
तदीयश्रवणात्सद्यो निर्बाधो बादरायणः ।।
(श्रीमद् भागवत महा. 2/73 )
महर्षि व्यासजी वेदों की संहिता बनाए, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रन्थों की भी रचना किए, ऋचायें लिखी, श्री महाभारत ग्रन्थ जिसमें सवा लाख श्लोक हैं, बनाया। इसमें गीता भी आ जाती है। इन सब संहिताओं का निर्माण किया और अपने शिष्यों को पढ़ाते रहे, परन्तु इतने पर भी उनके चित्त को शांति न मिली। चित उपराम न हुआ। वे बोधवान नहीं हुए। अज्ञान सागर में डूबे रहे।
भैया ! बुद्धि का व्यापार दूसरी चीज है! वेदों का सुनना सुनाना दूसरी बात है। परन्तु बोध प्राप्त करना, आत्म तत्व प्राप्त करना अलग चीज है। दर्शन, ब्रह्मसूत्र आदि की रचना करने पर भी जब श्री व्यासजी का चित्त शांत न हुआ तो वे सरस्वती नदी (शम्याप्रास) के तट पर (यह नदी हिमालय प्रदेश में है) खिन्न चित्त से बैठ गए। श्री व्यास जी ने अपनी इस अशांति को नारदजी के समक्ष रखा। उस समय देवर्षि नारद ने श्री व्यास जी के समक्ष इसी चतुःश्लोकी भागवत का प्रतिपादन किया। जिसे सुनकर महर्षि व्यास जी का चित्त प्रशांत हुआ, अज्ञान का नाश हुआ एवं वे निर्बाध हो गए।
तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्लोकसमन्वितम् ।
तदीयश्रवणात्सद्यो निर्बाधो बादरायणः ।।
जब भगवान नारद ने बादरायण (व्यासजी) को चतुःश्लोकी भागवत सुनाया, तब 'तदीय श्रवणात्सद्यो' अरे ! सुनते ही महर्षि व्यास जी निर्बाध अर्थात् संशय-विपर्यय रहित हो गए। निस्संकल्प हो गए अज्ञान का मूलोच्छेद हो गया। चित्त को परम शांति मिली। श्री शुकदेव जी ने यही चतुःश्लोकी भागवत। राजा परीक्षित को सुनाया था। यही विस्तार होने से अट्ठारह हजार श्लोकों का महापुराण ग्रन्थ बना। यही इसका प्रसंग है। अब हम सबसे यही कहते हैं कि आत्म कल्याण चाहो तो बिना कान के सुनो और बिना बुद्धि के समझो। स्वामी जी ! आप तो बड़ी अटपट बात बताते हैं, कहीं बिना कान के सुना जाएगा और बिना बुद्धि के समझा जाएगा? हाँ भाई ! यही तो हम बता रहे हैं। कान से जो सुनाई पड़ता है और जो कान से सुनाई नहीं पड़ता, कान के सुनने और न सुनने को जो सुनता है, वह किस कान से सुनता है? बुद्धि के समझने और न समझने दोनों को जो समझता है वह किस बुद्धि से समझता है? जो कान का कान है, बुद्धि की बुद्धि है, यारों! उसे कान क्या सुनेगा, बुद्धि क्या समझेगी। हाँ, चीज यही है। जो मन, बुद्धि, वाणी से परे है, उसको मन, बुद्धि वाणी से कैसे समझोगे? तो बस, जैसे बैठे हो, मस्त रहो।
कोई भी विद्वान संन्यासी जब अपने शिष्य मंडल को वेदांत का पाठ पढ़ाते हैं, उस समय गुरु परम्परा से गुरुओं का स्मरण करके वेदाध्ययन (वेदांत पाठ) कराते हैं। हम भी इसी गुरु परम्परा से आदि गुरुओं का स्मरण करते हुए वेदांत का निरूपण करेंगे।
ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरंच,
व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ।
श्री शंकराचार्यमथास्य पद्यपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् ।
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद् गुरुन सन्ततमानतोऽस्मि ।।
आत्मज्ञान के प्रथम आचार्य भगवान नारायण हैं। इनके बाद पद्मोद्भव (श्री ब्रह्मा जी) हुए। उनके शिष्य हुए श्री गुरुदेव वसिष्ठ। उनके शिष्य हुए महर्षि शक्ति और उनके शिष्य हुए पराशर। फिर इनके शिष्य हुए श्री व्यासजी और फिर शुकदेव स्वामी। जिनके शिष्य श्री गौड़पादाचार्य। उनके शिष्य श्री गोविंदपादाचार्य और इनके श्री आद्य जगद्गुरु भाष्यकार शंकराचार्य। उनके चार प्रधान शिष्य हुए हैं- पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य और त्रोटकाचार्य। इसी तरह गुरु परम्परा से अन्यान्य अध्यात्मतत्व के ज्ञाता श्रेष्ठ गुरु हुए हैं वे सभी आत्मरत, आत्मवित्, कृतकृत्य पद प्राप्त आनंदस्वरूप हुए हैं। भगवान नारायण से आदि लेकर जितने भी आज तक गुरु हुए हैं और भविष्य में होंगे, इन सब गुरुओं को हम अपने हृदय से स्मरण कर वेदांत का पाठ आरंभ करते हैं।
श्री भगवनानुवाच -
ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ।।
विज्ञान संयुक्तं तदङ्गं सरहस्यं मे परमगुह्य ज्ञान गृहाण ।।
हे ब्रह्मन् ! विज्ञान संयुक्त साङ्गोपाङ्ग क्या है? रहस्य क्या है? परम गुह्य क्या है। सूत्र रूप में इन सबकी व्याख्या की गई है।
'मैं' शरीर नहीं, आत्मा हूँ-यह है ज्ञान।
'मैं' सर्व हूँ-यह है विज्ञान ।
'मैं' हूँ-यह है परमगुह्य ज्ञान।
शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसका बोध होना ज्ञान और 'मैं' हूँ यह परमगुह्य ज्ञान है। देखो-जिस शब्द के साथ परम लगता है वह अपेक्षा रहित होता है। परम वैराग्य, परम पद, परम स्नेह, परम समाधि, परमानंद, परम सुख ये सब अपेक्षा रहित हैं।
ज्ञानं परमगुह्यं में यद्विज्ञानसमन्वितम् ।
सरहस्यं तदङ्ग च गृहाण गदितं मया ।।
भगवान कहते हैं- यह जो मेरा परमगुह्य ज्ञान है इसको ग्रहण करो। अरे ! मैं जो कहता हूँ उसको जानो, आत्मतत्व का अनुभव करो। यह अनुपम है। सम्पूर्ण अंगों के सहित ग्रहण करो। साङ्गोपाङ्ग क्या है? वेदांत के छः अंग हैं।
उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फले ।
अर्थवादपपत्तिं च लिंङ्गं तात्पर्य निर्णये ।।
उपक्रमोपसंहार, अपूर्वता, अभ्यास, फल, अर्थवाद और उपपत्ति ।
1. उपक्रमोपसंहार- जिस ब्रह्मतत्व का प्रपिादन किसी ग्रन्थ के अथवा विद्वान महान पुरुषों के भाषण आदि में किया गया है उसी का प्रतिपादन अंत में किया जाए। उसे उपक्रमोपसंहार कहते हैं।
2. अपूर्वता- 'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।' नहीं है ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरा पदार्थ। यह अपूर्वता है।
3. अभ्यास- अनेकानेक सुंदर-सुंदर युक्तियों द्वारा प्रतिपाद्य विषय के पुनः-पुनः निरूपण करने का नाम अभ्यास है।
4. फल- 'ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ।' देव को जानकर पंचक्लेश और अष्टपाश से जीव छूट जाता है। यह फल है।
5. अर्थवाद-
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च येन ।
अपार संवित्सुखगारेऽस्मिन् लीने परे ब्रह्मणियस्य चेतः ।।
स्नातं तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्तापिसर्वावनिर्यज्ञानां
च कृतं सहस्त्रमखिलं देवाश्च संपूजिताः ।
संसाराच्च समुद्धता स्वपितरस्त्रैलोक्य पूज्योऽप्यसौ
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् ।।
यह अर्थवाद है।
6. उपपत्ति - वासुदेवः सर्वमिति। यह उपपत्ति है।
जिस विद्वान महात्मा के उपदेशों में छः अंग नहीं रहेंगे तो जिज्ञासु को संशय-विपर्यय रहित पूर्ण रूप से आत्मतत्व का बोध नहीं होगा। इसीलिए यहाँ की कथा में इन छः अंगों का ध्यान रखा जाता है। ज्ञान निरूपण में छह अंगों का समावेश यथास्थान होता रहता है। जिसने अपने आपको जान लिया, आत्मतत्व का साक्षात्कार कर लिया। वह अष्टपाश, पंचक्लेश से छुटकारा पा जाता है। यह वेदांत का फल है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश ये जीव के पंच क्लेश हैं और घृणा, शंका, भय, लज्जा, निंदा, कुल, शील तथा जाति ये जीव के अष्टपाश हैं। असत को सत, चेतन को जड़ और दुःख को सुख यानी साढ़े तीन हाथ के शरीर को आत्मा मानना, यही अविद्या है। द्रष्टा और दृश्य के धर्मों को एक मानना यही अस्मिता है। इष्ट पदार्थ और वह जिसके द्वारा प्राप्त हों, दोनों के प्रति जो आसक्ति है, यही राग है और दोनों के प्रति जो घृणा है, यही द्वेष है। अनादिकालीन परम्परा से जिस मृत्यु प्रवाह से बड़े-बड़े विद्वान भी डरते हैं यही अभिनिवेश है। पंच क्लेश एवं अष्ट पाश से वही छुटकारा पा सकता है, जिसने अपने आप भगवान को पहिचाना है। यही वेदांत का फल है।
आत्मतत्व के विचार में यदि एक क्षण भी मन लग जाए, स्थिर हो जाए तो समस्त तीर्थों का स्नान उसने कर लिया। हजारों गौवों के दान का फल प्राप्त कर लिया, उसके पितरों का उद्धार हो गया। हजारों बार अश्वमेधादिक यज्ञ कर चुका, त्रैलोक्य का पूज्य हो चुका। अब जिसका चित्त परब्रह्म में लीन हो गया है उसका क्या फल है, उसकी क्या महिमा है? उसका कुल पवित्र हो गया। जननी जो माता है वह कृतार्थ हो गई, वसुंधरा जो पृथ्वी है वह ऐसे आत्मदर्शी को पाकर पुण्य रूप हो गई। इसको कहते हैं अर्थवाद। और उपपत्ति- 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन।' 'वासुदेवः सर्वमिति ।' भगवान आत्मदेव से एक तिल भर भी भिन्न नहीं है। एक ही चेतन परमात्मा है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वेदांत के चार अनुबंध होते हैं- अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन।
जिसको अपने आत्म कल्याण के लिए मछली के समान तड़प हो, आत्म तत्व को जानने की, प्राप्त करने की प्रबल जिज्ञासा हो वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। सर्व भगवान है, एक तृण भी भगवान से विलग नहीं, यही प्रतिपाद्य विषय है। प्रतिपादित विषय और उसका प्रतिपादक ग्रन्थ यही प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। आत्मतत्व का पूर्ण रूपेण साक्षात्कार करा देना यही वेदांत ग्रन्थ का प्रयोजन है। हाँ, जी! चलो आगे-
ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।
सरहस्यं तदङ्ग च गृहाण गदितं मया ।।
भैया ! परमगुह्य ज्ञान पर पहले प्रकाश डालेंगे नहीं तो विषय समझ में नहीं आवेगा।
कोई व्यक्ति जब कभी किसी महापुरुष के पास जाता है तो (चाहे शिष्टाचार के ही नाते कहता हो) कहता है कि भगवान! आप तो परम ज्ञानी हैं और में त अज्ञानी हूँ, तो महात्मा कहते हैं कि प्यारे ! यदि तू वस्तुतः अज्ञानी होता व अपने को अज्ञानी और मुझे ज्ञानी कैसे कहता? जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हर जा, मैं पागल हूँ तो क्या हम-तुम उसे पागल कहेंगे? जबकि उसे अपन पागलपन का ज्ञान है तो फिर वह पागल कैसे? इसी तरह जब वह व्यकि अपने को अज्ञानी कहता है तो वस्तुतः क्या वह अज्ञानी हुआ? अपने आपक अज्ञानी कहता है इससे यही सिद्ध होता है कि ज्ञान का स्वरूप जानकर अपने 'मैं' में अज्ञान को आरोपित करता है। वास्तव में तू अज्ञानी नहीं जबकि तुझे ज्ञान और अज्ञान दोनों का ज्ञान है। इसलिए तू स्वयं ज्ञान स्वर भगवान आत्मा है। अच्छा, ज्ञान, अज्ञान और इससे परे परम गुह्य ज्ञान।
मैं अमुक हूँ-अज्ञान, 'मैं' हूँ-ज्ञान, दोनों को जो जानता है उसे कहते परमगुह्य ज्ञान। नोट करो-
मैं अमुक हूँ-प्रगट ज्ञान, 'मैं' हूँ, गुप्त ज्ञान, इन दोनों प्रगट ज्ञान और गु ज्ञान के परिज्ञाता (जानने वाले) को परम गुह्य ज्ञान कहते हैं।
ये सब चीजें नारायण भाव में, नारायण द्वारा ही निकल रही है। अब क कसर तो नहीं रही, हृदय देश के भाव का हृदय देश से ही अनुभव हो सक है। जहाँ समझने की कोशिश किया तो सिर्फ साहित्य ही हाथ लगेगा। यहाँ आत्मतत्व का निरूपण, तत्व दर्शन हृदय से प्रवाहित हो रहा है और इसे ह से ही ग्रहण करो। यहाँ पर नारायण तत्व का निरूपण हो रहा, साहित्य निरूपण नहीं। समझो विषय- वेदांत का क्या स्वरूप है? वेद का अर्थ होता जानना। जिसको जानकर फिर जानना बाकी न रहे, उसे कहते हैं वेदांत। जान का अंत हो जाना, यही वेदांत है।
आत्म तत्व 'मैं' हूँ के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। उसी तत्व का प्रतिपादन हो रहा है। भैया! यह बुद्धि का विषय नहीं है। यह जो वेदांत्त है वस्तुतः भगवान आत्मा का ही कथन है। इसको वही कह रहा है और वही अनेकानेक रूप से सुन रहा है। यह तत्व बुद्धिगम्य नहीं है। यदि ' श्री भगवानुवाच' को 'अहं उवाच' कहें तो गलत न होगा। बस ! मैं अमुक हूँ, यह प्रगट ज्ञान है और 'मैं' हूँ, यह गुप्त ज्ञान है। अब इन दोनों का जो ज्ञान, वही परम गुह्य ज्ञान है। देखो-अभी अनुभव करो- समझो विषय को, मैं अमुक हूँ, इस अमुक भाव को जानकर ही तो कहोगे न कि वैसे ही बिना मतलब फालतू कह दोगे। बिना जाने कैसे कहोगे। अजी! जब वह अपने 'मैं' पर अमुक थोपेगा तो उसे जानकर ही तो कहोगे कि मैं देह हूँ आदि। उसे समझा है, परखा है, माना है तभी कहता है कि मैं देह हूँ, मैं संसारी जीव हूँ। अब देखो-इसमें 'मैं' अछूता है, अलग है, 'मैं' पर कोई कलङ्क नहीं है।
जितने यहाँ पर बैठे हो, इसे ठीक तरह से हृदयङ्गम कर लो। यहाँ पर कोई पंथ-पंथाई, मजहब या सभा सोसायटी की बात नहीं है। इनके दायरे के बाहर आओ। यहाँ पर कोई साम्प्रदायिक चीज नहीं बताई जा रही है। हम तो हिन्दुओं को ही नहीं, वरन् मुसलमान, जैन, ईसाई, वैष्णव, शैव सभी को उपदेश करते हैं। इन दायरों में क्यों पड़े हो? अरे ! मैं स्वयं अपने को कुछ मानकर ही तो इन दायरों में पड़ा हूँ। अरे राम, राम! बाहर जगत से संबंध तोड़कर आत्म जगत में आओ। बाह्य जगत को छोड़कर मैदान में आओ। युनिव्हर्सल टुथ (सार्वभौम सिद्धांत) सारे विश्व का एक होता है। इसमें कोई शंका नहीं। यदि अपना कल्याण चाहो, अपने कल्याण की तुम्हें भावना है और यहाँ से कुछ ले जाना चाहते हो तो विषय को हृदय से समझो। अपने व्यक्तित्व को अपने आपको जो माना है, उसका लोप करो। व्यक्तित्व को रखकर समझना चाहोगे तो तुम्हारे पल्ले कुछ न पड़ेगा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। व्यक्तित्व को लोप करके ही आत्म तत्व जान सकते हो। तो मैं अमुक हूँ, यह प्रगट ज्ञान है। मैं जानता हूँ कि मैं देह हूँ, जीव हूँ, इसलिए यह प्रगट ज्ञान है। तो क्या जानने वाला भी जीव है? जरा होश में आकर समझो। 'मैं' का आधार क्या जीव है? मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ यहाँ तक सब प्रगट ज्ञान है और 'मैं' हूँ यह गुप्त ज्ञान है और 'मैं' अर्थात् आत्मतत्व यही ब्रह्म ज्ञान है। इसको ग्रहण करो। इसका अनुभव करो।
ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ।।
आत्मतत्व का क्या रहस्य है? 'मैं' के रहस्य चार हैं। 'मैं' (आत्मा) का भाव। 'मैं' (आत्मा) का रूप। 'मैं' (आत्मा) का गुण और 'मैं' (आत्मा) का कर्म। आगे श्लोक में भगवान नारायण कहते हैं-
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः ।
तथैव तत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् ।।
(श्रीमद् भा. 2/9/31)
जैसा मैं हूँ 'मैं' का जैसा भाव, 'मैं' का जैसा रूप, 'मैं' का जैसा गुण और 'मैं' का जैसा कर्म, इन्हीं विषयों का ज्ञान 'मैं' आत्मा (आत्मतत्व) का रहस्य है। मेरी कृपा से इन तत्वों का अनुभव करो। अच्छा, विषय को पूर्णतया हृदयङ्गम करने के लिए प्रक्रिया सुनो। जो सत्संगी गण बाहर से आए हैं (छत्तीसगढ़ से) उनके लिए प्रक्रिया समझाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तो प्रक्रिया कहने से ही समझ लेते हो, परन्तु यह (झंडापुर स्थान) नवीन क्षेत्र है और नवीन क्षेत्र होने के कारण प्रक्रिया समझा देना आवश्यक हो जाता है। इसलिए पहिले जरा प्रक्रिया समझा दूं तब बाद में आत्म तत्व के भाव, रूप, गुण और कर्म का निरूपण करूँगा। साधारणतया 'मैं' का मतलब साढ़े तीन हाथ का शरीर ही मान रहे हैं, दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है। जिस तरह मक्खन दूध में व्याप्त है, परन्तु दूध में व्यापक होते हुए भी स्पर्श करने पर नहीं मिलता और जब उसी दूध का मन्थन किया जाता है तो मक्खन ऊपर आ जाता है। मक्खन की प्राप्ति दूध के मन्थन से होती है। इसी तरह विचार रूपी मथानी से इस मान्यता का मन्थन करें।
कोई अपने आपको साढ़े तीन हाथ का शरीर मानता है, कोई अपने आप को जीव मानता है तो कोई अपने आप को ब्रह्म मानता है। सभी अपने को एक ही विशिष्ट शरीर, जीव या ब्रह्म नहीं मानते। सभी मान्यताएँ विभिन्न-विभिन्न प्रकार की हैं। इन मान्यताओं को अलग करके समझा दूं। सुनो, ध्यान दो, पहले ये दो शब्द 'मैं' और 'मेरा' समझ लो। 'मैं' कर्तृवाचक है और 'मेरा' संबंध वाचक है। अपने आप के लिए, खुद के लिए 'मैं' कहा जाता है और अपने से संबंधित सम्बन्ध वाचक है। अपने आप के लिए, खुद के लिए 'मैं' कहा जाता है और अपने से संबंधित के लिए 'मेरा' का प्रयोग होता है। इस तरह मैं का अर्थ मेरा नहीं होता और न मेरा का अर्थ मैं होता है। अच्छा, यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तेरा नाम क्या है? वह कहता है मेरा नाम जगदीश है। भैया ! यह तो बताओ कि तुम्हारा नाम जगदीश कब रखा गया? तुम्हारे जन्म होने के पूर्व रखा गया था या तुम्हारे जन्म लेने के बाद? यदि तुम्हारा नाम जन्म लेने के पहले ही जगदीश होता तो जब तुम्हारा जन्म हुआ तभी तुम्हारी माँ पुकारती कि देखो जगदीश पैदा हो गया है। परन्तु, ऐसा कोई नहीं कहता। यह तो मौलिक बात है। तो नाम जन्म लेने के बाद ही रखा जाता है और कहते भी हो कि मेरा नाम, नाम 'में' मेरा शब्द लगा है। इसलिए यह स्वयं सिद्ध है कि मेरा कहने वाला नाम से अलग है। कुछ तुम्हें नई बात नहीं बताई जा रही है। साधारणतया सभी कहते हैं कि मेरा नाम, मेरा सिर, मेरी आँख, मेरी नाक, मेरा मुँह, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा शरीर। ऐसा कहने से ही सिद्ध होता है कि नाम से लेकर शरीर तक 'मैं' नहीं हूँ। हाँ जी, यदि मेरा का अर्थ मैं लगाऊँ तो?
किसी शहर में एक बड़े अच्छे पढ़े-लिखे धनवान व्यक्ति जमींदार साहब रहते थे। किसी दिन उसका पुत्र बीमार पड़ा। उसे डबल निमोनियो हो गया। उन्होंने अपने नौकर को आज्ञा दी कि फौरन अमुक डॉ. साहब को बुलाकर लावो। नौकर थोड़ी दूर जाकर कहता है कि सरकार ! यदि डॉ. साहब घर पर न हों तो? मालिक ने कहा जल्दी जाता है कि नहीं? हुजूर, मैं यह चला। फिर बाहर जाकर वापस आकर कहता है कि सरकार! डॉ. मिल भी गए और और दवाई न हुई तो? मालिक गुस्सा होकर कहता है कि अबे, जाता है कि नहीं? नहीं सरकार, चला जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। परन्तु, फिर वापस आकर कहता है कि सरकार ! यदि डॉक्टर साहब मिले भी, दवाई भी मिली, लेकिन यदि डॉक्टर साहब आने को तैयार नहीं हुए तो? जमींदार साहब गरम होकर बोले कि बेवकूफ कहीं का, जल्दी जाता है कि नहीं, बकबक कर रहा है। जल्दी ही डॉ. साहब को बुलाकर ला। हाँ सरकार अभी जाता हूँ। थोड़ी ही देर में फिर वापस कर कहता है कि यदि डॉ. साहब मिले भी, दवाई भी मिली और वे आने को तैयार भी हो गए, परन्तु उनके आने के पहले ही लड़का न रहा तो? भैया। इस, 'तो', का तो कोई इलाज नहीं है। यदि मेरा का अर्थ मैं लगाऊँ तो मैं गाड़ी हो जाऊँ, क्योंकि मेरी गाड़ी कहता हूँ। मेरी टोपी कहता हूँ, तो मैं टोपी हो जाऊँगा। इसलिए मेरा का अर्थ मैं नहीं।
आजकल जगह व जगह वेदांत के प्रचारक, वेदांत के ठेकेदार मिल सकते हैं, परन्तु ऐसे उपदेशक वेदांत का ठीक अर्थ नहीं लगाते। वे क्या भगवान की कथा करेंगे। भगवान को कभी देखे हों, उनका अनुभव किए हो तब न, भगवान को वे क्या लखावेंगे। वे तो भगवान को कभी सुने भी नहीं। मैं कथा नहीं करता, मैं वेदांत का प्रचारक हूँ। भगवान को देखना हो तो हमारे पास आवो। जब चाहो, जहाँ जाहो, जिस समय चाहो हम भगवान को लखा देने का दावा करते हैं। हम उन्हें अनुभव करा देंगे कि यही भगवान है। परन्तु, उन्हें भी भगवान के दर्शन की भूख हो तब न?
यदि किसी व्यक्ति को जिसे धन का लोभ है, कोई कहे कि भैया ! तुम्हें कोई काम न करना होगा। बिना कमाई के तुम्हें धन मिल जाएगा, तुम्हें लखपति बना देंगे, यदि तुम्हें धन की इच्छा हो तो दिला सकते हैं। तब तो सभी राजी हो जाएँगे, कहेंगे कृपा करो दादा, शीघ्रातिशीघ्र धनी बना दो। जब कोई काम ही न करना पड़े और धन मिलता हो तो सभी स्त्री-पुरुष तैयार हो जाते हैं। धन लेने के लिए शायद ही कोई बचे, सब तैयार बैठे हैं। हाँ भाई ! ऐसी ही बातें हैं। परन्तु, भगवान को पाने के लिए पता नहीं क्या नुकसान हो रहा है- राम ! राम !! घोर निद्रा से उठो ! जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस समय चाहो देखो। हम तुम्हें दिखा देंगे कि यही भगवान हैं। बस ! बाकी सब कुछ पाखंड है, गप्प बात है। हम विश्व के लिए चुनौती देते हैं। वह भगवान नहीं है, जिसे देखने के लिए तुम ज्योतिषियों से पूछकर मुहूर्त निकालकर मिलो । ज्योतिषियों के पास जाकर पूछो कि हमारी जन्मकुंडली देखकर बताइये कि हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं और यदि मिलेंगे तो कब मिलेंगे? भगवान ऐसे नहीं हैं कि इस तरह से मिलें।
कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ।।
(रा. उत्तर. कां.)
अरे! विषय भोग तो कूकर-सूकर भी करते हैं। विषय भोग उन्हें भी मिलता है। भगवान ने मनुष्य जन्म क्यों दिया? भगवान प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने शरीर दिया है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से ही होती है। मेरी नाक, मेरा कान, मेरा पैर, मेरा शरीर, हम सब यही कहते हैं और अंग्रेजी में भी 'माई बॉडी' कहते हैं, 'आई एम बॉडी' ऐसा तो कोई नहीं कहता। तो नाम से लेकर शरीर तक 'मैं' नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कहता हूँ और गौर करो तो शरीर मेरा भी नहीं है।
छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा ।
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ।।
(रा.कि.)
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पाँचों तत्वों के पंचीकरण से इस शरीर का निर्माण हुआ है। यह शरीर मल, मूत्र का भांड है। मरने-जीने वाला है। हाँ, यह अवश्य है कि 'मैं' इसके अंदर रहता हूँ और इसी गरज से मैं कहता हूँ कि मेरा कान, मेरी नाक, मेरा शरीर, परन्तु मेरा कहने की गरज से मैं शरीर नहीं हो जाता। तो समझ गए-वाह रे मिट्टी के शेर ! जिस तरह मैं नाक, आँख नहीं इसी तरह से शरीर भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शरीर कहता हूँ और जरा गौर से देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि शरीर मेरा भी नहीं है। जैसा मकान मिट्टी, गारे, ईंटों से बना है। इसमें खंभे, दरवाजे, बल्लियाँ, बांस, खपरे आदि लगे हैं। इसी तरह यह शरीर रूपी मकान मांस, मज्जा, अस्थि, रक्त आदि से बना है। हाथ-पैर रूपी खंभे लगे हैं। इसके नौ दरवाजे हैं। मकान में बल्लियाँ लगती हैं, इस शरीर रूपी मकान में हड्डी रूपी बल्लियाँ लगी हैं और चमड़ी से छाया गया है। मकान जिस तरह चूना, खड़िया, मिट्टी, गेरू, नीला थोथा आदि से पोता जाता है इसी तरह यह शरीर कोई काला, कोई गोरा, कोई साँवला है। जैसा वह मकान वैसा ही यह मकान है। तो फिर शरीर मेरा भी नहीं है। मांस, हड्डी आदि से बना है। पंच तत्वों के पंचीकरण से यह शरीर बना है। चूँकि मैं इसमें रहता हूँ, इसलिए रहने की गरज से मैं इसे अपना ही मान बैठा हूँ कि यह मेरा शरीर है।
याद रखो कि इस समाज में बड़े-बड़े विद्वान, वकील, न्यायाधीश बैठे हैं। ताजरात हिन्द के दफा 448 का जुर्म कर रहे हो। दूसरे के मकान में जबरदस्ती कब्जा करना अपराध है। तुम यह अपराध शरीर के विषय में कर रहे हो कि यह मेरा शरीर है, जबकि यह वस्तुतः पंचतत्वों का है। तुम पर यह दफा लागू होगा। यहाँ पर आत्मतत्व का निरूपण हो रहा है। आत्मा अपना आप 'मैं' है न कि शरीर। कमेटी के पंचों ने यह साढ़े तीन हाथ का मकान बनाकर तुम्हें दिया कि ले भैया इस शरीर को प्राप्त कर, इसके द्वारा प्रभु को प्राप्त करो। परन्तु, क्या इसे अपना ही समझ लिया और विषय भोग में पड़ गए। अरे! कूकर, शूकर भी विषय भोग करते हैं। तो यह मनुष्य का शरीर तुम्हें क्यों दिया गया? क्या विषय भोग के लिए? नहीं।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक संवारा ।।
एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गउ स्वल्प अंत दुःखदाई ।।
नरतन पाई विषय मन देहीं। पलटि सुधाते सठ विषलेहीं ।.
(उ.कां.)
शरीर मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए। परन्तु, वाह रे फतह बहादुर ! इस शरीर पर अपना कब्जा कर लिया, हम जैसा चाहें इस शरीर का उपयोग करें। अरे! तुम अनजाने दफा 448 का जुर्म कर रहे हो। हमारे पास इस संत कोर्ट में यह मामला आया है। इस कोर्ट में ऐसे मामले आते रहते हैं। याद रहे, इस कोर्ट में किसी की वकालत न चलेगी और यदि अभियुक्त हाजिर न हुआ तो एकतरफा डिग्री ठोंक देंगे। हाँ भाई ! फिर क्या, एकतरफा डिग्री ठोंक देंगे। तो हाँ, तुम्हारा दावा खारिज कर दिया गया। यह तो संतों की अदालत है। न तुम शरीर हो और न तुम्हारा ही शरीर है। न 'मैं' शरीर हूँ और न मेरा शरीर है। तो फिर हिन्दू, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, प्रणामी, उदासी, निर्मोही, निरंजनी, रामसनेही, कबीरपंथी, घीसापंथी, गोबरपंथी, कुंडापंथी आदि। अरे! इन्हें किस पर आरोपित करोगे? आजकल पंथों का भरमार लगा हुआ है। इस संसार में इस समय दो हजार नौ सौ निन्यानबे पंथ हैं और दिन-प्रतिदिन नए-नए बनते ही जा रहे हैं। अपनी- अपनी खंजरी और अपना-अपना राग। इन सभी पंथों में इनके अनुयाइयों में राग-द्वेष भरा पड़ा है। एक-दूसरे को पावें तो खा जाएँ और ऊपर से तारीफ, कि सभी पंथी अपने-अपने पंथ को अनादि मानते हैं। ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि इसके पंथ का जन्म आदिकाल का है। इनके जो धर्म प्रवर्तक हुए हैं वे सब आदि-अन्त वाले हैं। परन्तु दंभ तो देखो अपने पंथ को धर्म को अनादि बतलाते हैं।
राम-राम, तो भैया ! समझो मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, नीला हूँ, लाल हूँ, धर्मी हूँ, छह विकार वाला हूँ। छह उर्मियों वाला हूँ। ये सब शरीर के धर्म हैं। 'मैं' के नहीं, इस शरीर के हैं। शरीर जन्मता मरता है 'मैं' नहीं। मरना-जीना शरीर का धर्म है। इसीलिए जब 'मैं' इसे अपने पर आरोपित कर लेता हूँ तब इससे भयभीत रहता हूँ।
दो मित्र एक तीसरे मित्र के यहाँ गए। वह मित्र पूछता है कि आपके साथ जो आए हैं उनकी क्या तारीफ (परिचय) है? ये कौन हैं? तो वह मित्र कहता है- मित्र! ये हमारे क्लास फेलो हैं। ये हमारे साथ प्रायमरी में पढ़े, फिर हाईस्कूल में साथ-साथ पढ़े और कॉलेज में भी हम लोग साथ ही साथ पढ़े हैं। तब यहाँ प्रश्न होता है कि भाई! जब तुम प्रायमरी में पढ़े तो क्या तुम दोनों का यह दाढ़ी-मूंछ वाला शरीर ऐसा ही रहा होगा? तो कहता है कि नहीं। तब तो हम दोनों छोटे रहे। तो अब पहले जैसा शरीर न रहा, बदल गया और सोचो, जब 'मैं' शरीर होता तो 'मैं' भी बदल जाता, क्योंकि शरीर बदल गया है। जब 'मैं' भी बदल जाता तो यह याद किसको रहती कि ये हमारे सहपाठी हैं। इसलिए 'मैं' तो वही का वही हूँ, यद्यपि शरीर बदल गया है। शरीर बालक, युवा (जवान) बूढ़ा होता है और अन्त में मर जाता है, परन्तु शरीर के मर जाने से मैं आत्मा मरता नहीं हूँ। यह जो साढ़े तीन हाथ का ढ़ांचा दिख रहा है वह 'मैं' नहीं हूँ। यद्यपि 'मैं' रग-रग में बस रहा हूँ। मेरा नाम, मेरी नाक, मेरा मुँह, मेरा शरीर, यह सब मैं नहीं हूँ। अच्छा, देखो जो मैं कह रहा हूँ उसको न मानना, जो 'मैं' कहूँ उसको जानना। अरे यार! ये तो मस्तों के लतीफे हैं। जो मैं कहूँ उसको न मानना और जो 'मैं' कहूँ उसको जानना। यानी साढ़े तीन हाथ वाले की बात को न मानना यह जो व्याख्या से परे हैं उसको जानना। वह जो जानने की चीज है, मानने की नहीं। देखो-जो मानने की चीज है वह मरणधर्मी है, उसको माना जाता है। यहाँ पर सभी समझदार बैठे हैं। दोनों तरफ प्रकृति और पुरुष सभी विद्वत् समाज है। पंथों के पंडित जो हैं, वे अपने सेवक मंडल को अपने पंथ की बातें बताते हैं। उसी की व्याख्या करते चले जाते हैं, सेवक चाहे समझे या न समझे। बस, हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, मानते चले जाते हैं। हाँ, सत् वचन महाराज। जो उनके गुरु ने बताया, वही उनके धर्म हैं। परन्तु, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है। जब तक तुम्हारे गले के नीचे न उतरे, तब तक न मानना, नहीं तो पंथ-पंथाई आ जाएगी। सब बातें ठीक समझ लो फिर जानने का प्रयत्न करो। स्वामी जी ! आपने जो अभी बताया है इसका कोई प्रमाण भी है? जी हाँ, मैं प्रमाणित बात कहूँगा, ऊटपटांग बातें नहीं। इन सबका वेदोक्त प्रमाण है। प्रमाण सहित ही बताऊँगा, जो तुम्हारे चित्त को समाधान करेगा, जो शंकाओं का मूलोच्छेद कर देगा। यदि तुम्हारे चित्त को समाधान न हुआ तो स्वामीजी ठीक कह रहे हैं, यह न मानना। संसार में ठगों का जाल बिछा हुआ है, सम्हल-सम्हल कर पग रखना। पंथ और मजहबी पचड़े में मत पड़ो। यह सब समाज में ठगों का जाल बिछा हुआ है और लोग गुमराह हो रहे हैं। किस- किस की बात मानें, किसे ग्रहण करें? तो भैया ! चित्त को शांति तभी मिलेगी और हृदय में बात ठीक-ठीक बैठेगी, जब बात प्रमाणयुक्त होगी। तो 'मैं' न हाथ, न पाँव, न कान, न नाक और न शरीर, न मेरा शरीर। अच्छा तो स्वामीजी ! क्या 'मैं' सुन रहा हूँ? नहीं। मैं कहता हूँ कि मेरा मन-तो मैं मन भी नहीं। मैं कहता हूँ-मेरी बुद्धि, तो मैं बुद्धि भी नहीं। मेरा प्राण-मेरी सांस, तो मैं प्राण भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा जी घबरा रहा है, तो मैं जी भी नहीं। यहाँ तक कभी-कभी लोग कह देते हैं कि मेरी आत्मा-हालांकि मेरी आत्मा कहना ठीक नहीं, मेरी आत्मा कहना यह युक्तिसंगत नहीं है, आत्मा तो अपना आप है, आत्मा का अर्थ खुद होता है और 'मैं' का अर्थ भी खुद होता है तो 'मैं' स्वयं आत्मा हूँ। तो यह ठीक से समझ लो कि मैं और मेरा एक नहीं है।
यहाँ पर जो मुस्लिम भाई हों तो इस्लाम धर्म पर गौर करो। खुदा का क्या अर्थ होता है। खुदा की तशरीह क्या है, खुदा की व्याख्या क्या है? यहाँ पर हाफिज मौलवी सभी बैठे हैं। सभी से पूछता हूँ कि खुदा की क्या व्याख्या है।
खे दाल पेश-खुद, अलिफ साकिन- खुदा ।
खुद के मायने 'मैं'। जो दुनियाँ का खुद है, 'मैं' है वह एक है या अनेक ? एक है। अलिफ से एक लिखा जाता है। यही खुदा के मायने हैं-सारे जहान का, म.खलूक का जो खुद है, अलिफ मायने एक है। 'मैं' हूँ यह स्वामी जी अपने लिए कहते हैं ऐसा न समझना। अरे! कहाँ अंधेरे में भटक रहे हो। जरा प्रकाश में आओ यार ! अंधेरी न ढ़ोवो ! अंधेरी ढोने की बात जरा सुना दूं, बहुत दिन हो गए बताए-
कहीं एक भीलों की बस्ती थी। उन भीलों में दीपक जलाने का रिवाज नहीं था, रात्रि में दिया नहीं जलते थे। वरन् जब रात्रि होती थी तो गाँव के सभी भील, स्त्री-पुरुष अंधेरी ढोते थे। सिर पर गुड़री बना बड़े-बड़े टोकरों में अँधेरी को पैर से दबा दबा कर भर लेते थे और गांव के बाहर सड़क में फेंकते रहते थे। बालक, वृद्ध सभी सिर पर टोकरी लादकर अंधेरी फेंकते, यह क्रिया रात्रि भर चलती। जब सूर्य भगवान का प्रकाश दिखता, रात्रि बीतने पर जब अंधेरा स्वयं दूर हो जाता तो वे लोग समझते कि इन लोगों ने सब अंधेरी ढो डाली।
एक भील के लड़के की शादी किसी अन्य गाँव में हुई। नई दुल्हन घर में आई। नई बहू के घर में अंधेरी ढोने की प्रथा नहीं थी, वहाँ केलोग दीपक जलाते थे। जब रात्रि हुई तो उसकी सास एक बड़ी-सी टोकरी नई बहू के सामने रखकर उसको भी अंधेरी ढोने को कही। नई बहू सोचने लगी कि अच्छा पागलों के यहाँ आई हूँ। क्या अंधेरी भी कोई ढोने की चीज है? वह अंधेरी ढोने को राजी नहीं हुई। बुढ़िया बिगड़ गई, कहती है-चली बड़ी आई मेरी सास, मेरी सास की सास सभी अंधेरी ढोये हैं-चल उठ। इस तरह जब वाद-विाद हो रहा था तो घर का बूढ़ा ससुर आया और बीच-बचाव किया। उसने समाधान किया कि नई बहू आज ही आई है और थकी हुई है, इसलिए इसे अंधेरी ढोने को आज न कहा जाए। वरन् अपने पुत्र को कहा कि बहू के हिस्से की भी अंधेरी आज तू ही ढो देना। पुत्र आज्ञाकारी था, वह अपनी पत्नी के हिस्से की अंधेरी ढोने लगा। मुढ़ेरी बांधकर सिर में अंधेरी भरकर रात्रि भर ढोया। नई बहू दिन में पता लगा ली कि पास में बाजार कहाँ है-लोगों से मालूम किया कि चार-पाँच फर्लांग पर 'बिहार' नाम का एक गाँव है। हाँ भाई ! चश्मदीद मिशाल देनी चाहिए। नई बहू बाजार से दीपक, तेल, रूई सब ले आई और रात्रि में घर में दिवाली मनाई, घर जगमगा उठा। आगे-पीछे दशों दिशाओं में कहीं भी अंधेरी का पता नहीं। तब तो उसकी सास और सभी, बहू की पूजा करने लगे। यह तो साक्षात् जदगम्बा है। घर में जगत जननी आई है। उसका पति भी पाँव पड़ने लगा। घर में अंधेरी दूर हो गई और सभी घर में पैर फैला-फैलाकर सोये। यह बात जब गाँव के अन्य लोगों को मालूम हुई तो पूछने आए कि भाई ! आज तुम लोग अंधेरी क्यों नहीं ढोये? तब ये कहने लगे कि भैया ! घर में साक्षात् लक्ष्मी देवी आई है। बहू नहीं, साक्षात् जगदम्बा है, दिया के प्रकाश से अंधेरी का नाश बताए तो फिर गाँव का गाँव दण्ड प्रणाम करने लगे। देवी ! कृपा करो-हमारे घर की भी अंधेरी दूर कर देना। इस तरह इस गाँव से अंधेरी ढोने की प्रथा बंद हो गई। प्रकाश होने लगा।
यह तो एक दृष्टांत है। इसका द्राष्टांत है कि अनादिकाल से हृदय रूपी मकान में अज्ञान की अंधेरी छाई हुई है और इस अज्ञान रूपी अंधेरी दूर करने के लिए नाना प्रकार के साधन करते आ रहे हैं। कष्ट साध्य साधन कर रहे हैं परन्तु भैया ! जब तक कोई सद्गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत के शरण नहीं गए, उनकी कृपा नहीं प्राप्त किए तो अनादिकाल के साधनों में भी अज्ञानान्धकार समाप्त होने वाला नहीं। अज्ञान का नाश तो संतों की कृपा से ही होता है।
स्वामी जी ! यह दारुण अविद्या, जन्म-जन्म का अज्ञान, कैसे जल्दी से दूर हो! क्या कोई उपाय है कि अनादिकाल की अविद्या एक क्षण में दूर हो जाय ? कैसे होगा? इसका उत्तर सुनो-
किसी कन्दरा में हजारों वर्षों से अंधकार छाया हुआ है, अनादिकाल से अंधेरा है। वह अंधकार यह नहीं कहता कि हम जल्दी नहीं जाएंगे। यहाँ तो हमारा हजारों वर्षों का कब्जा है, लाखों बरसों का कब्जा है, जल्दी नहीं जाएंगे। परन्तु, ज्यों ही प्रकाश हुआ, एक दिया जलाया, त्यों ही वह हजारों वर्षों का अंधकार कहाँ चला जाता है, कितनी जल्दी अंधकार भाग जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं। इसी प्रकार यह हृदय का अंधकार, जन्म-जन्म का अज्ञान यह नहीं कहता कि हम नहीं जाएँगे। जब भी परम ज्ञान, ब्रह्मज्ञान का बोध होगा, अज्ञान का नाश स्वयं हो जाएगा। यह अविद्या रूपी अंधकार नहीं कहेगा कि हम नहीं जाएंगे। परम ज्ञान को प्राप्त करो। परम प्रकाश का अनुभव तुम स्वयं करोगे। इसलिए इस परम ज्ञान को प्राप्त करने की उत्कट जिज्ञासा जगाओ। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के समीप जाकर हाथ में पत्र, पुष्प, फल, समीधा लेकर उनके चरण में प्रणिपात होकर प्रार्थना करो। सद्गुरु के शरण में जाओ।
तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।।
(मुण्डक 1-2-12)
जिज्ञासुओं ! कान खोलकर सुन लो, नदी का बहना तब तक बंद न होगा जब तक कि नदी अपने घर में नहीं पहुँच जाएगी। नदी का घर समुद्र है और जब तक वह समुद्र में नहीं पहुँच जाती तब तक वह अचल नहीं होती।
सरिता जल जलनिधि महुं जाई। होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ।।
(रा.कि.)
लोगों की यह आम भावना हो गई है कि भैया! प्रारब्ध के बिना कुछ नहीं मिल सकता, तो फिर तकदीर के बिना भगवान को प्राप्त करना कहाँ संभव है। यह जान लो कि तकदीर के भरोसे न रहो। भगवान को प्राप्त करना तुम्हारे स्वयं के उत्कट अभिलाषा पर निर्भर है। यह गलत धारणा छोड़ दो कि तकदीर से, प्रारब्ध से भगवान मिलते हैं। भगवान तो तुम्हें स्वयं मिले हुए हैं।
उन्हें मंज़िल नहीं मिलती, जो किस्मत के सहारे हैं ।
उनकी ज़िन्दगी ही मौत, जो वै हिम्मत के हारे हैं ।। 1 ।।
जो बेग़र्जी से हैं जीते, उन्हें क्या मौत से डर है।
हमेशा खुद पे जो रोशन, वही रोशन सितारे हैं ।।2।।
हु.कूमत मुल्क पर थी जिनकी, वे दर-दर के भिखारी हैं ।
बिगड़ना बनना दोनों ही, ये कुदरत के नज़ारे हैं ।।3।।
जीना सच में उनका ही, जो खुद मस्ती में जीते हैं ।
सभी से 'मुक्त' हैं हरदम ये मस्तों के इशारे हैं ।।4।।
कौन? जो बंध से मुक्त और मोक्ष से भी मुक्त। सर्व सकंल्पों से जो मुक्त है। इसलिए-
जीना सच में उनका ही, जो खुद मस्ती में जीते हैं ।
सभी से 'मुक्त' हैं हरदम, ये मस्तों के इशारे हैं ।।
अरे ! ये मस्तों के लतीफे हैं।
उन्हें मंजिल नहीं मिलती, जो किस्मत के सहारे हैं ।
उनकी जिंदगी ही मौत, जो वै हिम्मत के हारे हैं ।।
ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ।।30 ।।
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः ।
तथैव तत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् ।।31 ।।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् ।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ।।32 ।।
ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ।।33 ।।
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु ।
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ।।34 ।।
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा ।।35 ।।
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ।
भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ।।36 ।।
(श्रीमद् भागवत 2/9/30-36)
प्रथम दिवस :
दूसरी बेला
दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक
प्रपन्न पारिजाताय तोत्त्रवेत्रैकपाणये ।
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः ।।
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।
देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ।।
मूकं करोति वाचालं पंङ्गं लङ्घयते गिरिम् ।।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम् ।।
प्रसंग चल रहा है- चतुःश्लोकी भागवत-
ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ।।30 ।।
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः ।
तथैव तत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् ।।31 ।।
विज्ञान समन्वितं संयुक्तं सरहस्यं च पुनः तदङ्गं मे परम गुह्यं ज्ञानम् हे ब्रह्मन् !
त्वं गृहाण। हे ब्रह्माजी ! विज्ञान संयुक्त यानी विज्ञान सहित साङ्गोपाङ्ग एवं रहस्य सहित मेरे परमगुह्य ज्ञान को तुम ग्रहण करो।
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्वविज्ञानं मदनुग्रहात् ते अस्तु । 'मैं' का जैसा भाव, 'मैं' का जैसा रूप, 'मैं' का जैसा गुण, 'मैं' का जैसा कर्म। हे ब्रह्माजी ! मेरी कृपा से चारों तत्वों का तुम्हें बोध वैसे ही हो जाए।'मैं' जैसा हूँ जो 'मैं' का भाव, रूप, गुण और कर्म। आओ, इन रहस्यों का अनुभव करें। भली-भाँति समझकर ग्रहण करो-अपने आप 'मैं' को शरीर से भिन्न समझो-यह पहले प्रक्रिया समझाने में बताई जा चुकी है। सूत्र रूप में जान लो कि जिन पदार्थों को मेरा कहता हूँ वह पदार्थ 'मैं' से अलग है। प्यारे ! जानों कि मेरा कहने वाला 'मैं' से अलग होता है।
समझो-यदि ऐसा कहा जाए कि 'मैं' ऐसा हूँ तो 'मैं' का प्रकार हो जाएगा क्योंकि यदि 'मैं' ऐसा हूँ तो ऐसा नहीं हूँ-ऐसा भी कहा जा सकता है, इसलिए 'मैं' ऐसा हूँ-ऐसा नहीं कहा जा सकता। 'मैं' जैसा हूँ वैसा ही हूँ। 'मैं' ही जानेगा कि वह कैसा है। यह दूसरी चीज है कि 'मैं' को कोई शरीर मानता है,
तो कोई जीव मानता है और कोई ब्रह्म मानता है, परन्तु 'मैं' तो एक ही हूँ। तो फिर इन विपरीत दृष्टि वालों को एक नहीं अनेक दिख रहा है। ये बात है मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा । 'यावानहं' की व्याख्या हो रही है।
जो जैसा है वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा ।।1।।
हूँ कौन कहाँ मैं कैसा, तशरीह नहीं तकरीर नहीं ।
हो गए मुसव्वर सब हैरां, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा ।।2।।
जितने भी वेद, पुराण, दर्शन शास्त्र हैं और उनके बनाने वाले ये सब चित्रकार हुए। ये सभी परेशान हैं 'मैं' को जानने में नेति-नेति कहते हैं, वहाँ मन, वाणी की गम नहीं।
अर्शे नकाब पोशीदा हूँ, दीदार ए चश्म पेचीदा हूँ ।
लग गए लबों पर चुप ताले, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा ।।3।।
अर्शे-आकाश, नकाब-घूंघट, पोशीदा-छुपा हुआ। मुझ भगवान आत्मा पर आकाश का पर्दा पड़ा है। 'मैं' कैसा हूँ यह दृष्टिगम्य नहीं है। आँख से तुम मुझे नहीं देख सकते। मुझे देखने में आँखें समर्थ नहीं हैं। 'मैं' पेचीदा हूँ।
सारी दुनियाँ का 'मैं' हूँ दुनियाँ फिर भी तलाश में फिरती है ।
बस यही तमाशा कुदरत का, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा ।।4।।
एक का नहीं सारी दुनियाँ का, जितने बैठे हो चाहे प्रकृति समाज हो या पुरुष समाज सभी अपने आपको क्या कहते हो? 'मैं'। तो सारी दुनियाँ का 'मैं' हूँ फिर भी दुनियाँ तलाश में फिर रही है। जन्म-जन्मांतर अनादिकाल से उस भगवान को ढूँढ़ रही है। भैया! यही तो माया का खेल है।
ये अजब अनोखी तसवीरें, खिंच रही तसव्वर में हरदम ।
तसवीर तसव्वर दोनों को, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा ।।5।।
ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सभी 'मैं' हूँ और उसकी तस्वीर खिंच रही है। अरे ! किसमें देख रहो हो? किस पर सारा संसार खिंचा हुआ है।
ये अजब अनोखी तसवीरें, खिंच रही तसव्वर में हरदम । ओ। हो।
तसवीर तसव्वर दोनों को, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा ।।5।।
देखा तो सभी ने-फिर देखने वाले को भी, क्या देखा? क्योंकि तसवीर और तसव्वर एक ही है। देखने वाले अनेक हैं पर देख किस को रहे हैं? एक को। स्त्री देखती है कि यह मेरा पति है। पुत्र देखता है कि यह मेरा पिता है। बहिन देख रही है कि यह मेरा भाई है। चाचा देखता है कि यह मेरा भतीजा है। साला के लिए यह बहनोई है। शत्रु देखता है कि यह मेरा शत्रु है। मित्र देखता है कि overline 45 मेरा मित्र है। तसवीर एक ही है, परन्तु देखने वाले भिन्न-भिन्न देख रहे हैं। इस साढ़े तीन हाथ के शरीर का बँटवारा अभी तक न हो सका। इसके हिस्सेदार अनेक हैं। पत्नी का पति, पुत्र का पिता, ये भाव उन्हीं के पास है। यदि यह शरीर सचमुच में पति होता तो फिर सबको ही वह पति ही दिखता। तब तो वह सबका ही पति हो जाएगा, सभी स्त्री उसे पति मानते हैं। तो बहिन का भाई बहिन के पास है।
तसवीर तसव्वर दोनों को, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा ।।
'मैं' तो आत्म तत्व तसव्वर इसको क्या देखा?
यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो,
बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैय्यायिकाः ।
अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः,
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ।।
जिस 'मैं' आत्मा को शैव शिव रूप से उपासना करते हैं। किसकी? मैं आत्मा की। जिस आत्मा को बौद्ध बुद्ध नाम से उपासना करते हैं। नैयायिक जिसे कर्ता मानकर उपासना करते हैं। जैन जिसे अर्हन्तदेव कहते हैं। कर्मवादी जिसे कर्म मानकर उपासना करते हैं। इसलिए कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा।
अरे ! जो 'मैं' यही तसव्वर है। यही तुलसी का राम है। सूर का श्याम है। गोपियों का कृष्ण है, मीरा का गिरधर है। हिन्दुओं का जो ईश्वर है। मुसलमानों का जो खुदा है। ईसाइयों का ईसा है। यहूदियों का मूसा है। बौद्धों का बुद्ध है। जो आस्तिकों का 'है' है और नास्तिकों का 'नहीं' है।
कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा-
'मैं' जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। देखो-अज्ञानवश अनादिकाल से मोह निद्रा में सोने वालों! क्या समझे? आत्मा को साढ़े तीन हाथ का शरीर माना है, उसे जीव माना है, भैया! यह 'मैं' क्या हूँ-इस महत्व को समझो -
प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्ध बोध स्वभावः
सदसदिदमशेषं भासयन्निर्विशेषः ।
विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववस्था,
स्वहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः ।।
(विवेक चूड़ामणि-137)
जो प्रकृति और विकृति से परे है यानी जो परमात्मा न किसी का कारण है, न किसी का कार्य है। न परमात्मा किसी से पैदा हुआ है और न परमात्मा से कुछ पैदा हुआ है। अगर मान लो कि परमात्मा किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो फिर यह पता लगाना होगा कि वह किससे पैदा हुआ है और फिर उसका पैदा करने वाला किससे पैदा हुआ? तो यहाँ पर वेदांत का चक्रिकापत्ति दोष आ जाएगा और फिर जब परमात्मा पैदा हुआ तो शायद कहने वाला पुरुष तो देखा ही होगा कि वहाँ जब पैदा हुआ, पैदा होने के टाइम में मानो वहाँ खड़े हों, बुद्धि से समझो-इसलिए परमात्मा किसी से पैदा नहीं हुआ। जब परमात्मा से भी कुछ पैदा नहीं हुआ। अर्थात् संसार पैदा ही नहीं हुआ। जिज्ञासुओं ! देखो-अरे! अभी पोल खोल देते हैं-परमात्मा न जन्मने वाला है, न जन्म देता है। कारण, जो जन्म लेता है, वह मरता भी है।
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।
(तैत्त.उप.)
फिर उसे कैसे जन्मने वाला मानें? जो जन्म रहित है, अनन्त है वह कैसे जन्म लेगा जब सब कुछ वही है। जो स्वयं जन्म लेना नहीं जानता तो पैदा क्या करेगा? अरे भाई! हाँ-उसे क्या तमीज होगी जो जन्मना नहीं जानता, वह दूसरे को क्या पैदा करेगा? देखो-जिसने तुमको पैदा किया वह भी किसी से पैदा हुआ था-तो फिर उसका जन्म देने वाला उसका बाबा और उसका जन्म देने वाला वह भी किसी से पैदा हुआ था और इसीलिए तो तुमको भी पैदा करने की तमीज है-इसलिए इनसे कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्ध बोध स्वभावः-प्रकृति-विकृति से परे, शुद्ध बोध ही जिसका स्वभाव है, अशुद्ध बोध नहीं। तो क्या स्वामीजी ! अशुद्ध बोध भी होता है? हाँ, क्यों नहीं- वह भी होता है। मैं अमुक हूँ, फला हूँ-यह अशुद्ध बोध है। 'मैं' का 'मैं' ही हूँ-यह शुद्ध बोध है। ' प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्ध बोध स्वभावः सदसदिदमशेषं भासयन् निर्विशेषः' जो सत है न असत है। विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववस्था- जो जाग्रत अवस्था में विलास करता है, जो स्वप्नावस्था में विलास करता है, जो सुषुप्ति अवस्था में विलास करता है। जो तीनों अवस्था में समरूप से विलास करता है। जाग्रत अवस्था में कैसे विलास करता है? जो जाग्रत अवस्था के प्रपंच को जानता है। यहाँ पर स्त्री समझ बैठी है, यहाँ पर पुरुष समझ बैठा है, इसे कौन जानता है? इसका कौन साक्षी है? इसको कौन देखता है? यही परमात्मा का जागृदादिक अवस्था का विलास है। यही परमात्मा बुद्धि का साक्षी, शरीर के अंदर अहमिति 'मैं' हूँ 'मैं' हूँ इस शब्द के द्वारा जो निरंतर अभिव्यक्त हो रहा है।
यहाँ पर सभी विद्वान बैठे हैं-इसका अर्थ लगाओ, भाव समझो अहमिति- निरंतर जो आवाज हो रही है- 'मैं' हूँ 'मैं' हूँ। स्वहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः। जो मन का साक्षी है, जो बुद्धि का साक्षी है, जो चित्त का साक्षी है।
प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्ध बोध स्वभावः,
सदसदिदमशेषं भासयन् निर्विशेषः ।
विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववस्था,
स्वहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः ।।
(विवेक चूड़ामणि)
इसलिए मैं आत्मा ही हूँ। इसी को समझ लो। बस, इतना ही। यहाँ पर सभी विद्वान, शिक्षक वर्ग बैठे हैं। हम लोग जब चौथी पढ़ते थे तो ग्रामर में पढ़ते थे-संभव है यह आजकल छठवीं में पढ़ाते हों-ग्रामर में तीन प्रकार के पुरुष पढ़े-उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष । सः, त्वम्, अहम् । वह, तू, मैं वह-अन्य पुरुष है, तू-मध्यम पुरुष है और मैं उत्तम पुरुष है-यह बताया गया। गुरुजी ने इसी तरह से शिक्षा दी कि बेटा! ध्यान देना, 'मैं' अधम पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष है। मैं साढ़े तीन हाथ का पुतला मल-मूत्र का भांड-अधम पुरुष है और इसके अंदर 'मैं' हूँ वह उत्तम पुरुष है। तो भैया ! यह ज्ञान एकदेशीय नहीं वरन् व्यापक है। हाँ, भाई! वेदांत तो सभी को सिद्ध करता है।
उत्तम पुरुष-ठीक से पढ़ना-पुरुष जो उत्तम है वह, अपने 'मैं' को जान लिया और वह पुरुषोत्तम हो गया। पुरुषोत्तम क्यों? क्योंकि वह समझदारी से, ज्ञान से, आत्म तत्व के विचार से अपने आपको जाना। अरे ! वह जो जाग्रत का जानने वाला है, स्वप्न को जानता है, सुषुप्ति को जानता है और मूर्छा को जानता है, समाधि के आनंद का अनुभव करता है, समाधि के टूटने को जानता है, मूर्छा के बेहोशी को जो जानता है-
यहाँ पर बड़े-बड़े डॉक्टर बैठे हैं। वे बतावें कि जब वे कोई सीरियस बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो वे रोगी को दो-तीन घंटे बेहोश रखते हैं। तो यह प्रश्न होता है कि श्रीमान् जी ! उस दो-तीन घंटे की बेहोशी को कौन जानता है? यदि 'मैं' बेहोश हो जाऊँ तो बेहोशी को कौन जानेगा? शरीर तो हमेशा ही बेहोश है तो फिर वह क्या जानेगा। डॉ. लोग क्लोरोफार्म सुंघाते हैं और इस तरह तुम्हें बेहोशी में लाकर शरीर का चीर-फाड़ करते हैं। हाँ, मन को ही सुख-दुःख अथवा पीड़ा होती है, इसलिए उसे ही बेहोश किया जाता है। 'मैं' तो सदैव साक्षी रूप से देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए इस बेहोशी का साक्षी 'मैं' ही हूँ और कौन होगा। तो क्लोरोफॉर्म किसको सुंघाते हैं? मन को। मन बेहोश रहता है, 'मैं' बेहोश नहीं होता। कारण? मुझे आत्मा में होश-बेहोश दोनों नहीं है। 'मैं' कारण, कार्य से परे हूँ।
तो फिर समझ लो। समाधि के उदय अस्त को 'मैं' जानता हूँ। 'मैं' मर्यादा से विचलित नहीं होता। सब समय एक रस रहने वाला हूँ। शाश्वत हूँ। इसलिए overline 45 मैं आत्मा 'विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववस्था' पुरुषोत्तम हूँ और उसी का प्रतिपादन यहाँ हो रहा है। यही वेदांत है, अध्यात्म विद्या है। तो 'मैं' जैसा है वैसा ही है-उसे किसी ने देखा नहीं-
वाह, जी वाह- कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा-
बेदाल लाम वाले मैं को, बेदिल होकर जिसने देखा ।
हो गया मुक्त जंजालों से, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा ।।6।।
दाल भात नहीं-
दाल जेर लाम-दिल, हिन्दी में जैसे अ, इ, उ की मात्रा ऐसे ही उर्दू में जबर, जेर, पेश है। मुझ आत्म देश में दिल गायब है। दिल नाम की कोई चीज नहीं।
हो गया मुक्त जंजालों से, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा ।।
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः ।
तथैव तत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् ।।
जैसा 'मैं' का भाव, जैसा मैं का रूप, जैसा मैं का गुण, जैसा 'मैं' का कर्म-मेरी कृपा से तुम्हें इन तत्वों का बोध हो जाए। चतुःश्लोकी भागवत के अंतर्गत कुल सात श्लोक हैं। दो श्लोक प्रस्तावना है, चार श्लोक मूल भागवत है और अन्त एक श्लोक इसकी फलश्रुति है।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् ।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ।।
ऋतेऽर्थंयत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ।।
सुनो, आज के पहले भी 'मैं' ही था। यह नहीं कि आज ही हूँ। आज के पहले भी 'मैं' ही था और आज के बाद भी 'मैं' ही रहूँगा। यहाँ पर आत्मा की व्याख्या हो रही है। इसका विवेचन पहले शास्त्रीय पद्धति से कर लें फिर युक्तियों से बोध कराएंगे।
'स्थूल, सूक्ष्म, कारण देहादव्यतिरिक्तो अवस्थात्रयसाक्षी
सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठति सैव आत्मा ।।'
स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों से परे, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी, सत्, चित्त, आनंद रूप से जो स्थित रहे वही आत्मा है। जाग्रत अवस्था में स्थूल शरीर जान लो, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर जान लो और सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर जान लो। इन सबसे परे, परे का अर्थ यह नहीं किसी तरह से अलग कहीं और। परे का अर्थ, इनके गुण, धर्म से परे आत्मा हूँ इसके अंदर होते हुए भी इनके धर्मों से परे अलग और जाग्रत, स्वप्न, सुषप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी, सत् चित् आनंद स्वरूप, इन सब अवस्थाओं का अनुभव करने वाला 'मैं' आत्मा हूँ। इसी को युक्ति द्वारा सुनो-जिसके बिना जो नहीं सिद्ध हो, जिसका अस्तित्व जिसके बिना न रहे, वही उसकी आत्मा है। एक क्षण भी जिसके बिना जो नहीं रह सकता, वही उसकी आत्मा है। देखो-यह डंडा है-यदि डंडा लकड़ी से कहे कि मैं तुमसे अलग हूँ तो यह सिर्फ अभिमान होगा, क्योंकि डंडे की आत्मा लकड़ी है। सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं। इसलिए सूत, कपड़े की आत्मा है। आभूषण स्वर्ण के बिना नहीं इसलिए स्वर्ण आभूषण की आत्मा है। 'मैं' आत्मा सर्व का सर्व हूँ। सारे जहान का वजूद, उसकी हस्ती, उसकी सत्ता 'मैं' आत्मा ही हूँ। जी हाँ-
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् ।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ।।
आज के पहले भी 'मैं' ही था परन्तु 'मैं' न सत् था न असत् था-था जरूर। क्या प्रमाण कि आज के पहले मैं ही था? इसका प्रमाण 'मैं' के सिवाय और कौन होगा। अरे! 'मैं' ही प्रमाण हूँ। जैसे किसी ने कहा कि मेरी जिह्वा नहीं है-तो फिर भैया ! तुम बोल कैसे रहे हो? सुनो, आज के पहले 'मैं' था, 'मैं' नहीं था, 'मैं' के था और 'मैं' के नहीं था को जो था उसने देखा या जो नहीं था उसने देखा? हाँ और समझो भैया ! बिना अपने बयान के मुलजिम छुटकारा नहीं पाता। आज के पहले 'मैं' नहीं था। 'मैं' के भाव, अभाव का साक्षी 'मैं' ही तो था। ओहो ! 'मैं' के अस्तित्व की अनुभूति 'मैं' ही करता हूँ। मैं की महिमा का कथन वेद, शास्त्र सभी करते हैं, परन्तु मेरा कथन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मन, वाणी का विषय नहीं हूँ। भगवान कहते हैं-आज के पहले भी 'मैं' ही था और आगे भी 'मैं' ही रहूँगा। अरे भाई ! भगवान की जन्मकुंडली को क्या कोई जानता है? 'मैं' हूँ 'मैं' नहीं हूँ, 'मैं' था, 'मैं' नहीं था, 'मैं' रहूंगा, 'मैं' नहीं रहूंगा इत्यादि। का साक्षी 'मैं' ही तो हूँ। यदि 'मैं' न रहूँ तो मेरी व्याख्या कौन करे? भाव को अभाव बताना यही व्याघात दोष है। यहाँ पर वेदांत का व्याघात दोष आ जाएगा। यदि कोई कहे कि मेरा पिता अखण्ड ब्रह्मचारी है। है तो तुम क्या आकाश से पैदा हुए हो? मेरी जिह्वा नहीं है, तो तुम कैसे बोल रहे हो? इसलिए आज के पहले भी 'मैं' था, आज के बाद भी 'मैं' ही रहूँगा और अभी भी 'मैं' ही हूँ।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् ।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ।।
किसी भी पदार्थ (दृश्य) को देखकर चार कल्पनाएं पैदा होती हैं-देश, काल, वस्तु और कर्ता। वह पदार्थ कोई न कोई देश में बना, किसी न किसी समय में बना, किसी न किसी वस्तु से बना और इसका कोई न कोई बनाने वाला होगा। इसी तरह जब हम संसार को ढूँढते हैं कि संसार कब बना, इसको किसने बनाया, कैसे बना, कहाँ बना आदि तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि संसार एक विकल्प है।
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ।।
(योग दर्शन) शब्द सुनने में तो आवे परन्तु ढूँढ़ने पर वस्तु न मिले, उसे कहते हैं विकल्प। विकल्प भाव शून्य है। विकल्प को ढूँढ़ने चलो तो हाथ कुछ न लगेगा। जब डंडा विकल्प को ढूँढ़ने चलेंगे तो हाथ में लकड़ी ही स्पर्श में आती है, परन्तु डंडा कहीं नहीं मिलता। इसी प्रकार संसार सुनने में तो आ रहा है, परन्तु संसार कहाँ है, कैसा है, कुछ पता नहीं लगेगा। संसार को ढूँढ़ने पर इसका पता ही न मिलेगा।
व्याकरण के अनुसार गम्लृ गतौ धातु से जगत शब्द सिद्ध होता है।
मैं तोहि अब जान्यौं संसार।
ज्योंकदली तरुमध्य निहारत, कबहुंन निकसत सार ।।
(विनय पत्रिका)
कदली के वृक्ष के खंभे को परत-परत निकालते चलो, फिर चाहे अंत तक निकाल डालो। कुछ भी न मिलेगा। एकदम पोलमपोल-कुछ भी नहीं। साधारणतया सभी पूछते हैं कि भैया! कौन गाँव से आये हो? आगन्तुक कहता है-भैया ! हम सब झंडापूर से आए हैं। समझना सभी आसपास पढ़े-लिखे बैठे हैं। हम कहते हैं कि भैया! उस झंडापुर को हमें हाथ से पकड़ा दो कि यही झंडापुर है। देखो, क्या सामने जो महुआ का वृक्ष है वह झंडापुर है? ऐसी कोई भी जगह हमें बताना जिसे झंडापुर कहकर पकड़ा सको और तारीफ यही है कि पटवारी के खाते में झंडापुर ही लिखा मिलेगा, परन्तु यदि उसे खोजने जाओ तो वह झंडापुर न मिलेगा यही संसार है। इसको विकल्प कहते हैं। इसलिए झंडापुर में रहने वाले अपने आप सभी झंडापूर है। सब बड़ा गड़बड़ गड़बड़ है। यही विकल्प है। झंडापुर ढूँढ़ने पर नहीं मिलेगा।
('जो दिखता है वह दिखता है, मैं दिखता हूँ तब दिखता है। इस रहस्य को जान लिया तब दिखना कहाँ जो दिखता है।)' देखने वाला ही तुमको दिखता है। दिखने वाला और देखने वाला यदि वस्तुतः भिन्न-भिन्न हैं तो देखने वाले को निकाल लो तो भी दिखने वाला दिखे तब अलग-अलग मान सकते हो। परन्तु, उसका तो अस्तित्व ही नहीं रहता इसलिए दिखने वाला, देखने वाले से भिन्न नहीं है। तो देखने वाला ही दिखता है। 'मैं' देखता हूँ, तब दिखता है, क्योंकि अस्तित्ववान तो 'मैं' ही हूँ। इस रहस्य को जान लिया तो फिर दिखना कहाँ जो दिखता है।
क्या-क्या कह डालूँ यार! हमको इतना उत्साह है कि क्या-क्या बता दूँ- चाहे सुनने वाले को इतना उत्साह न हो, परन्तु यहाँ तो उत्साह है। हाँ, जी! जिस प्रकार मेले में एक लाख व्यक्ति जमा हैं। जब कोई मेले में जाकर मेला को खोजे कि मेला कहाँ है? जिससे पूछो कि भैया ! कहाँ आए हो? तो यही उत्तर मिलता है कि मेला देखने आये हैं? बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब मेला देखने आए हैं? यदि किसी व्यक्ति से पूछो कि महाराज ! क्या आप मेला देखने आए हैं? श्रीमान् जी जरा हमें बताना कि मेला कहाँ है? मेला में दुबे, तिवारी, चौबे, पाण्डेय सभी आये हैं, परन्तु सबकी बोलती बंद है। मेला को बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, परन्तु बोलते सभी हैं कि मेला देखने आए हैं। तब फिर मेला कहाँ है? जिस-जिस से पूछो, वे सब के सब मेला देखने आए हैं. ऐसा कहते हैं पर वास्तव में वे सब स्वयं ही मेला हैं। इसी प्रकार संसार प्रपंच का देखने वाला मैं आत्मा स्वयं प्रपंच हूँ। जिस प्रकार मेला देखने वाले से मेले की सत्ता भिन्न नहीं है, इसी प्रकार प्रपंच का देखने वाला मुझ आत्मा से प्रपंच की सत्ता भिन्न नहीं है। यहाँ पर कोई साम्प्रदायिक बात नहीं है। यह युनिव्हर्सल टूथ (व्यापक सत्य) है, कोई बाजारु चीज नहीं है।
सिद्ध करना है-देश, काल, वस्तु और कर्ता। लकड़ी से डंडा, किवाड़ (दरवाजे) चौखट आदि बनते हैं, परन्तु इन सबमें व्यापक तत्व लकड़ी ही है। लकड़ी खिड़की नहीं है, कुर्सी नहीं है। अरे! जिसे अपने अस्तित्व का (लकड़ी का) ही परिज्ञान नहीं वह क्या जानेगा कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है।
यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञात् स्याद्वाचारम्भणं
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।।
(छा.उप 6/1/14)
अर्थात् जिस प्रकार एक मृत्तिका पिंड के जान लेने से मिट्टी से बने हुए समस्त घटादिक पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, यानी सब मिट्टी ही हैं। घट आदि विकास तो केवल कथन के ही लिए हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है। मिट्टी के बर्तन को हाथ लगाओगे तो मिट्टी ही हाथ लगेगी इसलिए मृत्तिका का ज्ञान हो जाने पर जितने मिट्टी के बने हंडी, दिया, परई आदि सभी का परिज्ञान हो जाता है। रामायण तो सभी पढ़ते हैं। जब रामायण का पाठ करते हो तो इस पद पर ध्यान क्यों नहीं देते-
आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नभवासी ।।
सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रणाम जेरि जुग पानी ।।
क्योंकि सभी सीय राममय है। राम व्यापक तत्व है। जितने गीता के पाठ करने वाले हो क्यों नहीं निम्न श्लोक पर ध्यान देते-
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिंदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।।
(गीता 7-7)
जब सभी वासुदेव है। वासुदेवः सर्वमिति । जरें-जरें से यही आवाज आ रही है। मुसलमान भाई लाइलाह इल्लिल्लाह कहते हैं। अर्थ क्या है-नहीं है अल्लाह के सिवाय दूसरा कुछ भी।
नाम, रूप ही संसार है और यह वाणी का विकार है।
यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञात्ꣲ᳭ स्याद्वाचारभ्भणं
विकारोनामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ।।
(छा.उप. 5/1/15)
अर्थात् जिस प्रकार लोहे के एक टुकड़े का ज्ञान हो जाने पर लोहे से बने समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है (यानि ये सब शस्त्रादिक तो लोहा ही है), उसी प्रकार नाम, रूप तो केवल वाणी के विकार मात्र हैं, सत्य तो लोहा ही है।
सारे चराचर का आधार परमात्मा राम है जो सर्व का सर्व है। उससे तो तुम्हें वैराग्य हो गया है। आत्मा से तुम वैराग्य लिए बैठे हो और विषय से प्रेम, तो फिर तुम्हें कैसे समझ में आएगा। सर्व का मूल तत्व, सर्वाधार, निर्विकार, कोई भिन्न चीज नहीं है। अपना आप 'मैं' आत्मा, चाहे आत्मा कहो या परमात्मा-
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सद्मत्परम् ।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ।।
बस, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। शीघ्रातिशीघ्र विकल्प को हटाओ। यह जगत विकल्प है और विकल्पाभाव 'मैं' आत्मा हूँ और इसी जगत रूपी विकल्प के अभाव में भगवान है। इसलिए विकल्प का अभाव कर दो। फिर जो बाकी रहा वह आत्मा ही आत्मा है। आत्मा से यारों! भिन्न कुछ भी नहीं। क्या-क्या बताएँ। 'मैं' का भाव, 'मैं' का रूप, 'मैं' का गुण, 'मैं' का कर्म।
अज्ञानसंज्ञौ भवबंधमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात् ।
अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ।।
(श्रीमद्भा. 10/14/26)
प्रश्न है कि चराचर का विकल्प क्या है और विकल्प का अभाव क्या है? सुनो-विकल्प भाव जगत है और विकल्पाभाव भगवान आत्मा है। वाह जी, वाह आज इसी का बोध करा दें। भैया! हमारे यहाँ कथा नहीं होती, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, यह है एक चलता-फिरता अध्यात्म विद्या का विश्वविद्यालय। यहाँ पर अध्यात्म की पढ़ाई होती है। ध्यान दो कि यदि कल की पढ़ाई समझना हो तो आज की पढ़ाई पक्की कर लेनी चाहिए। अध्यात्म (आत्म तत्व) के विद्यार्थियों को यहाँ पर बिला नागा यही लखाया जाता है। यदि तुम्हारे मन में आत्म तत्व को जानने की प्रबल जिज्ञासा है, यदि आत्म स्वरूप लखना चाहते हो, यदि तुम्हें 'मैं' का साक्षात्कार करने की उत्कट अभिलाषा है, तब हम दावे के साथ कहते हैं कि जब यहाँ से जाओगे तो अज्ञानी होकर नहीं, वरन् बोधवान होकर ही जाओगे। अच्छा तो भगवान ने सबसे प्रथम किस चीज का विकल्प किया? भगवान आत्मा पर किसका विकल्प सर्वप्रथम हुआ?
जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग्विधान् ।
वाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः ।।
(गौ.पा.मा.का.वै.प्र.-16)
सबसे प्रथम भगवान (परमात्मा) ने अपने आप में जीवभाव का विकल्प किया। सबसे शुरू में विकल्प किया कि मैं अज्ञानी जीव हूँ और यह सबसे बड़ा विकल्प है। जीव हूँ, इस विकल्प से छुटकारा पाना ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होना है। जीव विकल्प के बाद अनेक विकल्पों का जाल बिछ गया। विकल्प पर विकल्प होते गए। जीव ने प्रपंच का जाल बिछा दिया। फिर संसार दिखने लगा। पुत्र, पौत्र, पुत्री, मामा, दादा, दीदी आदि भाव (विकल्प) पैदा हो गए। लकड़ी पर डंडे का विकल्प होते ही फिर अनेक विकल्पों का उद्भव होने लगा कि इस डंडे का कोई न कोई बनाने वाला होगा। यह डंडा कहीं न कहीं बना होगा। किसी काल में बना होगा, किसी वस्तु से बना होगा। देश, काल, वस्तु और कर्ता का विकल्प हो गया। इसी तरह विकल्पों का जाल बनते चला। इसी तरह भगवान आत्मा मैं पर जीव भाव का विकल्प होते ही इस सृष्टि को किसने बनाया, यह सृष्टि कब बनी, इस सृष्टि का कर्ता कौन है? पालन-पोषण करने वाला कौन, इसका संहार करने वाला कौन है। इत्यादि विकल्प पैदा हो गए। अस्तित्वहीन भासना ही विकल्प है।
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ।।
(योग दर्शन)
शब्द का तो ज्ञान हो, परन्तु वस्तु का अभाव हो यानी केवल शब्द ही सुनने में आवे, परन्तु ढूँढ़ने पर जिसका अस्तित्व किसी काल में न मिले, उसे कहते हैं विकल्प। मतलब यह कि अस्तित्वहीन वस्तु को ही विकल्प कहते हैं। सभी प्रकार का विकल्प जीव भाव में निहित है। जीवभाव गया तो सभी विकल्पों का नाश स्वयमेव हो गया। जीवभाव के जाते ही विकल्पों का जाल सिमट गया, सब लोप हो गया। नहीं तो इन्हीं विकल्पों में पड़े रहो और इसी में बन्ठाढार है। भाई! विकल्प असत्य है। वह अस्तित्वहीन होता है। सुनो, जीववादियों ! जीव विकल्प है, अस्तित्वहीन, सोलह आने, इसमें कोई शक नहीं करना। अच्छा, क्या समझे? स्वामी जी! वही जो आपने समझाया।
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा ।।
मेरे दर्शन का यह परम अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जीव का सहज स्वरूप क्या है? अपना आप मैं भगवान आत्मा ही जीव का सहज स्वरूप है। सहज स्वरूप किसको कहते हैं? जो स्वरूप सनातन हो, व्यापक हो, अखण्ड हो। तो जीव का सहज स्वरूप जीव नहीं है। अरे ! यह तो विकल्प है। प्रभु के दर्शन का यही फल है कि वह आत्मा 'मैं' को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा को प्राप्त कर लेना ही फल है। हाँ जी, जीव का वास्तविक स्वरूप जीव नहीं है, यह तो विकल्प है। जीवभाव वैकल्पिक है, जो सत्ताहीन होता है और इसी जीवभाव में अनेकानेक विकल्प निहित हैं और आत्मभाव में सभी विकल्पों का नाश है। आनंदमानन्दकरं प्रसन्नं-
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् ।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ।।
ऋतेऽर्थंयत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ।।
ऋते-बिना, यत् अर्थ प्रतीयेत् आत्मनि न प्रतीयेत् तद् आत्मनो मायां विद्यात् अर्थ के बिना जो प्रतीत होता है और जिसमें प्रतीत होता है, वास्तव में वह उसमें (आत्मा में) प्रतीत नहीं होता। हाँ भाई! समझने वाले की मौत है। देखो-समझो विषय-विषय जरा सूक्ष्म है। देखना किसको कहते हैं और प्रतीत होना किसको कहते हैं? जिसको मैं आत्मा जानता हूँ वह प्रतीति है। प्रतीति अहं गम्य है। जो इन्द्रियग्राह्य है वह दृश्य है और जो इन्द्रिय ग्राह्य है वह इदं गम्य होता है। अहं गम्य 'मैं' हूँ और इन्द्रिय गम्य जगत है। देखो, यह माइक्रोफोन है, इसे विकल्प कहें कि वस्तु ? भैया ! माइक्रोफोन विकल्प है। विकल्प सत्ताहीन होता है। वह अस्तित्ववान नहीं होता। विकल्प हटा दो... विकल्प के हटाने पर क्या यह रहेगा? कुछ नहीं...। विकल्पाभाव 'मैं' हूँ और यही प्रतीति है. विकल्पभाव जगत है। अरे भाई! देखो, डंडा विकल्प है, इसे लकड़ी से हटा दो, विकल्प के हटते ही डंडा का अभाव हो गया। इसलिए पहले विकल्प का नाश करो। रामायण में क्या आप लोग नहीं पढ़ते-
गो गोचर जहं लगि मन जाई। सो सब माया जानेहू भाई ।।
इन्द्रियाँ गौवें हैं और उन गौवों के चारे पाँचों विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं। तो पहले विषय का विकल्प होता है कि इन्द्रियों का? विषय का विकल्प पहले होता है, उसके बाद इन्द्रियाँ उन विषयों को ग्रहण करती हैं। यह तो साधारण सी बात है, भैया! पहले गाय खरीदते हो कि पहले चारा का बन्दोबस्त कर लेते हो तब गाय खरीदते हो, पहले क्या करते हो? चारे का बन्दोबस्त पहले करते हो और फिर गाय खरीदते हो। इसलिए विषय पहले होता है फिर इन्द्रियाँ पैदा होती हैं। यह बहुत मार्के का विषय है, ध्यान देकर सुनो-
(पू. श्री स्वामीजी हाथ से ताली बजाकर शब्द विषय का अनुभव कराते हैं।) प्रेम से सुनो, यह गहन तत्व है। समझो हाँ हम तो भैया! इसके ही लिए सिर मुड़ाये हैं। बाबा बनने का कारण क्या है? और समझाऊँ? इन्हीं विषयों में इन्द्रियाँ जाती हैं। जब ये विषय आते हैं तो इन्द्रियाँ उतावली होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। तो सबसे पहले विषय का विकल्प होता है। (स्वामी जी ताली बजाते हैं) देखो, अभी शब्द विषय का विकल्प मत करो- तो इस अवस्था में यह शब्द विषय-विषय न होकर भास रहता है, यह प्रतीति है और इसका अनुभव मैं आत्मा से ही हो रहा है। अब शब्द विषय का विकल्प करो। शब्द विषय का विकल्प होते ही कर्ण इन्द्रिय इसे ग्रहण करेगी। इस शब्द विषय को चरने के लिए पशु रूपी कर्ण इन्द्रिय प्रेरित हो जाएगी। ग्राह्य और ग्राहक इसे भी समझ लो। ग्राह्य विषय और ग्राहक इन्द्रियाँ ये दोनों एक ही काल में पैदा होते हैं और दोनों विकल्प हैं। यदि शब्द विषय नहीं तो कर्ण इन्द्रिय भी नहीं। इन्द्रियाँ खायेंगी क्या? मर न जाएंगी। जब चारा नहीं तो पशु कैसे जीवित रहेंगे? जब विषय का विकल्प करते हो तब उस घास रूपी विषय को खाने के लिए इन्द्रियाँ प्रबल हो जाती हैं। यह बड़े तत्व की बात है। ये इन्द्रियाँ बड़ी बलवान हैं। किसी मैदान में चारा डाल दो तो क्या जानवरों को उसे खाने के लिए न्यौता देना होगा? अरे भाई! नहीं वे स्वयं आ जाते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार यह जगत विषय है और जगत विकल्प के अत्यन्ताभाव में इन्द्रियाँ आँख, कान, नाक, पैर आदि नहीं रहेंगे। यही तो तूष्णी पद है, अनिर्वाच्य पद है। यही 'मैं' का रूप है। अहा !!!
जगत (प्रपंच) किसको कहते हैं? संसार को बिना जाने-समझे हठयोगी कान में रूई दूँसते हैं कि कहीं शब्द विषय का भान न होने लगे जिससे कि बाह्य जगत विषय मन में न आए। उसे विकल्प से भय लग रहा है। समझो अरे भाई! विकल्प है ही नहीं। इसका नाम अध्यात्म है। और क्या देखते हैं? किससे बचने के लिए योगी ध्यान लगा रहे हैं। अरे! जो है ही नहीं। आया समझ में।
ऋतेऽर्थंयत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ।।
तभी तो ईशावास्योपनिषद (यह यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय है) के प्रथम मंत्र में-
ॐईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ।। ईशा. 1।।
इदं सर्वम् ईशावास्यम्। यह जो कुछ है सब ईश्वर है। जो कुछ भी जगती में जगत है-जगती है-जगती का अर्थ है भास (प्रतीति) और इस भास पर जो विकल्प उसे कहते हैं जगत, वह सब भगवान आत्मा है।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ।।
कस्य स्विद्धनम् - अर्थात किसी के अर्थ को ग्रहण मत करो यहाँ पर धनम् को पैसा रुपया नहीं समझना। वरन् धनम् को 'अर्थम्' समझना। एवं ज्ञात्वा भुञ्जीथा-ऐसा जानकर भोग करो। अर्थ को क्यों ग्रहण करते हो जबकि अर्थ ही लगाने में दुःख है। चलो, तुम्हें उदाहरण देकर समझाएँ कि अर्थ से ही दुःख होता है।
एक गाँव में कोई किसान अपने खेत को जोत रहा था और साथ ही बैलों के मालिक की लड़की को गाली भी दे रहा था। हाँ भाई! हल जोतने वाले का यह भजन है। स्वाभाविक अंड-वंड बकते रहते हैं। उसी खेत के पास से एक श्रीमान् जी निकल पड़े और गालियों को सुनकर वहाँ खड़े हो गए। किसान उन्हें खड़ा देखकर पूछा कि श्रीमान् जी क्या देख रहे हो? वह बोला कि मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि तू बैलों के मालिक की लड़की को गाली दे रहा है, तो बैलों का मालिक कौन है? किसान ने कहा बैलों का मालिक तो मैं ही हूँ। तब फिर यह गालियाँ किसको पड़ती होंगी? वह तपाक से बोला-जो बेवकूफ इस गाली का अर्थ लगाता होगा उसी को गाली पड़ेगी। हम तो अपने स्वभाव में कहे जा रहे हैं।
तो स्वभाव भाव जगती और 'अर्थ' भाव जगत। अमुक भाव मान्यता है इसलिए अमुक भाव को त्याग करके भुञ्जीथा। भोग करो। जहाँ' अरे' है वहीं अटक है, जहाँ अटक है वहीं खटक है, जहाँ खटक है वहीं भटक है और जहाँ भटक है वहीं लटक है। 'अरे' भाव अपने हृदय से निकाल दो। तो इस श्रुति के मंत्र का भाव लगा कि नहीं। देखो, यदि कोई शंका हुई कि अरे ! ऐसा मैंने क्यों कहा-बस ! इस अरे में ही अर्थ भाव है, न कि भास में (प्रतीति में)। बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं और उनसे पुण्य-पाप कार्य होते रहते हैं, परन्तु उनके मन में इस पुण्य-पाप की कोई रेखा नहीं पड़ती। 'अरे' आता ही नहीं। स्वभाव में खेल रहे हैं। बच्चे बरसात के दिन में कभी मेढ़क पा जाएँ तो उसके पैर में रस्सी बांधकर दिन-दिन भर घसीटते रहते हैं, खेल में उसे पटक भी देते हैं। अंततोगत्वा उसे मार भी डालते हैं, परन्तु बच्चों के मन में 'अरे' नहीं होता। हाँ 'अरे' उसको होते हैं जो बालक के रक्षक होते हैं। रक्षक वर्ग कहते हैं कि बच्चों ऐसा न करो, तुमको पाप लगेगा, क्योंकि वे अर्थ लगाते हैं। भैया! अर्थ में 'अरे' है।
ॐईशावास्यमिदंꣲ᳭ सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ।।
मान्यता, अर्थ विकल्प ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थ अथवा जगत भाव-कस्य स्विद्धनम् मा गृधः-अरे! किसी के अर्थ को ग्रहण मत करो। इत्येव ज्ञात्वा भुञ्जीथा-बस, स्वभाव में रहो।
ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ।।
ऊपर के इन दो श्लोकों में 'मैं' का भाव और 'मैं' का रूप सुना। अब 'मैं' का गुण सुन लो।
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु ।
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ।।
जिस प्रकार पंच महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी) सब भूतों में हैं भी और नहीं भी हैं। पंच महाभूत और उनके कार्य रूप भूतों को समझो। पांचो तत्व इसमें प्रविष्ट भी हैं और अप्रविष्ट भी। तो फिर जगत भाद में पांचों तत्व निहित हैं और यदि इन पाँचों तत्वों को इससे अलग कर लें, निकाल लें तो क्या रहेगा और किसमें रहेगा? इसलिए ये पंच महाभूत अपने कार्य में प्रविष्ट भी हैं और अप्रविष्ट भी हैं। इसी प्रकार 'मैं' आत्मा सर्व में हूँ भी और नहीं भी हूँ। अन्वय भाव से 'मैं' सर्व में हूँ और व्यतिरेक भाव से नहीं भी हूँ। यही 'मैं' का गुण है।
कार्येषु कारणत्वेनानुवृत्तिरन्वय ।
कारणावस्थायां च तेभ्यो व्यतिरेकः ।।
कार्य में कारण की जो व्यापकता, वह अन्वय है और कारण में कार्य का जो अत्यन्ताभाव, वह व्यतिरेक है। जो हो उसे कार्य कहते हैं और जिससे हो उसे कारण कहते हैं। डंडा कार्य है और लकड़ी कारण है। कार्य रूप डंडे में कारण रूप लकड़ी व्यापक है, यह अन्वय है और कारण रूप लकड़ी में कार्य रूप डंडे का अत्यन्ताभाव है, यह व्यतिरेक है। अन्वय रूप लकड़ी में कार्य रूप डंडे का अत्यन्ताभाव है, यह व्यतिरेक है। अन्वय रूप से लकड़ी डंडे में व्याप्त है और व्यतिरेक भाव में लकड़ी में डंडा नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए डंडा कहाँ? क्योंकि डंडे का अस्तित्व तो कारण रूप लकड़ी से है। तो अपने आप 'मैं' आत्मा को जानने के लिए अन्वय और व्यतिरेक है और जगत (प्रपंच) को जानने के लिए अध्यारोप और अपवाद है। अध्यारोप और अपवाद का प्रसङ्ग पीछे कहेंगे। मैं आत्मा सर्व में व्यापक हूँ, यह अन्वय है। मुझ आत्मदेश में प्रपंच का अत्यन्ताभाव है, यह व्यतिरेक है। यानी मुझ आत्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज हो तो 'मैं' उसमें व्यापूं। जब 'मैं' परिपूर्ण हूँ तो कहाँ रहूँ? यही भाव रामायण में भी है-
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना ।।
यह अन्वय है।
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अनुभवगम्य भजहिं जेहि संता ।।
यह व्यतिरेक है।
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा ।।
एतावदेव जिज्ञास्यं-इतना ही जानना जिज्ञासुओं के लिए जिज्ञास्य है। भगवान नारायण ब्रह्माजी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन् ! इससे अधिक कुछ नहीं जानना है। बस इतना ही जिज्ञास्य है। इसे अन्वय और व्यतिरेक द्वारा जानो। आज के पहले भी 'मैं' ही था और इसके बाद भी 'मैं' ही रहूँगा और आज भी सर्व 'मैं' ही हूँ। जो कुछ स्थावर जङ्गम चराचर है वह सर्व 'मैं' ही हूँ। बस ! इससे अधिक जानने की जरूरत आत्म जिज्ञासु को नहीं है। इतना ही जान लेना है और यही आत्मा 'मैं' का कर्म है।
अब यहाँ शंका होती है कि भगवान आत्मा में, जो सर्व में प्रस्फुटित, प्रस्फुरित है, सर्व में अभिव्यक्त हो रहा है, कर्म कहाँ? 'मैं' आत्मा का स्वरूप तो अक्रिय है और यहाँ पर आत्मा में कर्म भाव? यह तो आत्मा पर कलङ्क है। क्या आत्मा द्वारा भी कार्य होता है? समाधान-
अरे भाई ! यह आत्मा पर कलङ्क नहीं है। शिव.... जानना ही जिसका स्वरूप है-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-इति श्रुति प्रमाणत्वात्।' जो नित्य ज्ञान स्वरूप है। मुझ आत्मा को किसी वस्तु को जानने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। किसी उपकरण द्वारा जाना जाय तो वह कर्म कलङ्क है। सूत्र लिखो- "किसी उपकरण द्वारा कुछ भी करना यह कर्म कलङ्क रूप है और किसी उपकरण द्वारा कुछ जानना, यह भी कर्म कलङ्क रूप है। बिना उपकरण द्वारा जानना यह कर्म स्वरूप ही है।" आँख का देखना, आँख का कर्म नहीं है, स्वभाव है। देखना और आँख क्या दो हैं? जी नहीं, देखना और आँख भिन्न-भिन्न नहीं है। अब आ गई बात समझ में? किसी भी तरह देखो, कान के सुनने, न सुनने को जो सुनता है-दोनों का अनुभव करता है, दोनो को जानता है, तो यह जानना ही मुझ आत्मा का कर्म है जो कि मुझ आत्मा का स्वरूप ही है। आँख के देखने, न देखने को जो देखता है, तो वह कर्म स्वरूप ही है इसलिए कलङ्क नहीं है। यही 'मैं' आत्मा का कर्म है।
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा ।।
चतुःश्लोकी भागवत के इन चार श्लोकों में पहले श्लोक में 'मैं' आत्मा का भाव दूसरे श्लोक में 'मैं' आत्मा का रूप, तीसरे श्लोक में 'मैं' आत्मा का गुण और चौथे श्लोक में 'मैं' आत्मा के कर्म की विवेचना की गई है। अन्त के श्लोक में इनकी फलश्रुति बताई गई है।
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ।
भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ।।
ब्रह्माजी ! यह जो मैंने सिद्धांत आत्मतत्व के विषय में बताया है उसमें तुम सम्यक् प्रकार से परम समाधि करके स्थित हो जाओ, टिक जाओ। सब ओर से इन्द्रियों के कर्म को त्याग कर आत्मनिष्ठ बनो-केन प्रकारेण? परम समाधिना- परम समाधि के द्वारा-इसमें टिक जाओ। परम समाधि किसको कहते हैं? देखो-हठयोग में प्राण की समाधि होती है। राजयोग में चित्त की समाधि होती है। ज्ञानयोग में वासना की समाधि होती है। ये सभी समाधियाँ जिस अवस्था में समाधिस्थ हो जाती हैं, उसे परम समाधि कहते हैं। परम समाधि को भक्तियोग कहते हैं। हाँ-यही भक्ति है। आत्मदेश का ही नाम भक्तियोग है। भगवान इसी आत्मदेश में सम्यक् प्रकार से टिकने के लिए कहते हैं। अरे ! मैं अमुक हूँ इस अमुक भाव को छोड़कर, मान्यता जगत से रहित होकर, परम समाधि में टिक जाओ। यही इसका फल है और फिर जब तुम कालान्तर में प्रपञ्च की रचना करोगे तो तुम्हें शोक, मोह नहीं होगा। मस्त रहोगे। भगवान नारायण ने परमेष्ठी ब्रह्माजी को इस प्रकार आत्म तत्व का साक्षात्कार कराया।
द्वितीय दिवस
भगवान नारद एवं राजा प्राचीनबर्हि संवाद द्वारा कर्मो का विश्लेषण, राजा पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव ईश्वर एकता का विश्लेषण
19-2-1969, प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
श्री नारायणोपनिषद् पाठ।
अजमपिजनियोगं प्रापदैश्वर्य योगादगतिच
गति मत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं ।
विविध विषय धर्म ग्राहि मुग्धे क्षणानां
प्रणतभय विहन्तृ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ।।
प्रपन्न पारिजाताय तोत्त्रवेत्रैक पाणये ।
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः ।।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणुरमर्दनम् ।
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ।।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदमाधवम् ।।
अनन्त नाम, रूपों में अभिव्यक्त, अहमत्वेन प्रस्फुरित, महामहिम, स्वात्मस्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित आत्म जिज्ञासुगण। 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत ।' अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवो ! 'उत्तिष्ठत'- उठो स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो, किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में उपसन्न होकर अपना आत्म कल्याण करो।
यहाँ पर श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता के माध्यम से अध्यात्म तत्व का निरूपण हो रहा है। कल के प्रसङ्ग में राजा परीक्षित का अभिशापित होना एवं गंगा तट पर श्री स्वामी शुकदेवजी का आगमन एवं परमेश्वर नारायण द्वारा ब्रह्मा के प्रति चतुःश्लोकी भागवत का उपदेश प्रतिपादन हुआ। इस समय का प्रसङ्ग भगवान नारद एवं राजा प्राचीनवर्हि के संवाद में आत्म तत्व (विमल ज्ञान) का उपदेश है। सुनो, प्रेम से-
न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः ।
ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः ।।
(श्रीमद् भागवत 4/25 / 5 )
गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थधीः ।
न परं विन्दते मूढो भ्राम्यन्संसारवर्त्मसु ।।
(श्रीमद् भागवत 4/25/6)
राजा प्राचीनवर्हि भगवान नारद से प्रश्न करता है कि हे महाभाग। कर्मापविद्धधीः परं आत्मानं अहं न जानामि । येन ज्ञानेन कर्मभिः मुच्येयः त विमलं ज्ञानं माम् प्रति ब्रूहि। अनादिकाल से कर्म-कलिल में मेरी बुद्धि सनी हु है इसलिए भगवान आत्मा को मैं नहीं जानता। आप मेरे प्रति उस विमल ज्ञान का उपदेश कीजिये जिससे कि मैं कर्मजाल से छुटकारा पा जाऊँ। आत्म जिज्ञासुओं ! कर्म काण्डी की बुद्धि आत्म तत्व का विचार नहीं कर सकती। कारण, कि कर्मकांडी देहात्मवादी होता है। वह अपने को साढ़े तीन हाथ वाला मानता है। जब वह अपने को साढ़े तीन हाथ वाला न मानेगा तो उसके द्वारा कर्म नहीं होगा। कर्मकाण्डी की बुद्धि देहात्मवादी होने के कारण स्थूल होती है। उसका अन्तःकरण, उसके विचार, उसके संकल्प और उसके कार्य सभी सीमित और देहभाव में ही होते हैं। बात स्पष्ट है कि जब कर्मकाण्डी अपने को साढ़े तीन हाथ वाला मानता है तो उसकी बुद्धि, विचार, अन्तःकरण कर्मआदि सभी साढ़े तीन हाथ वाले ही तो होंगे। यह निर्विवाद सिद्धान्त है कि वह इसी शरीरी भाव तक ही सीमित होता है। तो हे महाभाग ! कर्मजाल में मेरी बुद्धि सनी हुई है इसलिए आत्म तत्व का विचार करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। अतः आत्म तत्व का कृपया विवेचन करें। कर्मकाण्डी वेदांत की उपेक्षा करता है। क्यों न ऐसा हो, वे तो वेदांत को समझते ही नहीं और यही (कारण है कि वे वेदांत के अनुयायियों की खिल्ली उड़ाते हैं, जिसकी बुद्धि सीमित है, साढ़े तीन हाथ की है वह भगवान नारायण आत्म तत्व के सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव को क्या प्राप्त करेगा जबकि अहम् ('मैं') शब्द करके भगवान आत्मा प्रत्येक शरीरों में प्रस्फुरित प्रस्फुटित एवं अभिव्यक्त हो रहा है। जिस भगवान आत्मा के समक्ष आकाश सूक्ष्मातिसूक्ष्म होते हुए भी सुमेरु पर्वत के समान स्थूल है उसे कर्म में फँसी हुई स्थूल बुद्धि क्या समझेगी।
न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः ।
ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः ।।
इसलिए राजा प्राचीनबहिं प्रश्न करता है कि जिस ज्ञान से कर्मों में फँसी हुई बुद्धि कर्मजाल से छूट जाती है, ऐसे विमल ज्ञान का प्रतिपादन कीजिए।
विमल ज्ञान का भाव और उसका विश्लेषण-
इस कथन से यह सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं मल संयुक्त ज्ञान भी होता है। हाँ, विमल की अपेक्षा मल सहित। तो मल सहित ज्ञान क्या है?
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई ।।
देखो, जमें रहो, जहाँ के तहाँ अपने आप 'मैं' आत्मा को 'मैं' के साथ आत्मा शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 'मैं' का भाव और आत्मा एक ही है। चाहे आत्मा कहो या 'मैं'। 'मैं' का अर्थ आत्मा के सिवाय कुछ नहीं, परन्तु इसे जोड़कर कहा जाता है, क्योंकि साढ़े तीन हाथ वाले शरीर को भी मैं का संबोधन लोग करते हैं। साधारणतया मैं का अर्थ साढ़े तीन हाथ का शरीर मान लेते हैं इसलिए मैं के साथ आत्मा कह दिया जाता है। नहीं तो 'मैं' कहना काफी है। स्वस्वरूप आत्मा को मैं अमुक अमुक हूँ ऐसा मान लेना यानी अपने 'मैं' को कुछ न कुछ मान लेना ही मलिन ज्ञान है। जानता तो है परन्तु विमल नहीं, मल सहित, क्योंकि माना हुआ ज्ञान है और मान्यता के हटते ही 'मैं' का 'मैं' शुद्ध भाव रह जाता है। यही विमल ज्ञान है। इसी को भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं-
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।।
(गीता 7-25)
योगमाया समावृतः (आच्छादित) अहं आत्मा सर्वस्य न प्रकाशः - मैं आत्मा योग माया करके आच्छादित यानी ढँका हुआ सबको प्रकाशित नहीं होता। सब मुझे नहीं जान सकते, क्योंकि योगमाया से ढँका हूँ। पहिले इस ढक्कन को तो समझ लो भगवान का घूंघट क्या है? योग माया। विद्वज्जनों ! माङ्-माने धातु से माया शब्द बनता है। अरे यार ! जो माना जाय वह माया। 'ममीते विश्वमिति या सा माया'- मोहित कर लिया है विश्व को जिसने, उसे कहते हैं माया।
गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थधीः ।
न परं विन्दते मूढो भ्राम्यन्संसारवर्त्मसु ।।
कर्मकाण्डी क्या कहते हैं? जप करो, तप करो, तीर्थ व्रत करो, दान, पुण्य करो। जब तुम्हारा यह शरीर छूट जाएगा तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम स्वर्ग तो जाओगे। वस्तुतः यह सकाम कर्म का उपदेश अज्ञानियों को कर्म में प्रवृत्त करने का साधन है। इसे कूटधर्म अथवा पुष्पिता वाणी कहते हैं।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।।
(गीता 2-42)
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफल प्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।।
(गीता 2-43)
भैया ! स्वर्ग से कुछ नहीं होता। हाँ, यदि स्वर्ग जाना हो तो तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दानादिक करो, मरने के बाद विमान आएगा। हाँ, जी-तैयारी में बैठे रहो। आज दिन तक तो स्वर्ग गए लोग-स्वर्ग जाकर कभी किसी के नाम, इष्ट मित्रों स्वजनों के नाम चिट्ठी नहीं लिखे कि उन्हें वहाँ अच्छा मकान मिला है, घर की खबर ठीक रखना, तिल्लो, धान वगैरह ठीक से बोना और पत्र देते रहना- ऐसा कोई पत्र नहीं देता। तो कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति भले हो, परन्तु आत्म तत्व के बोध बिना अज्ञान का नाश नहीं होता। यह स्वयं सिद्ध है-इसी को तत्व कहते हैं। यही तत्व है। मानो तब भी है, न मानो तब भी है। तो-
न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः ।
ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः ।।
(श्रीमद् भागवत 4/25/5)
कर्मकाण्ड-जन्म, कर्म से छुटकारा नहीं देता, जन्म, कर्म फल देने वाला है। पुण्यी, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और जब पुण्य क्षीण होगा तो-फिर ! वही-
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।।
(गीता 9-21)
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।।
(गीता 2-43)
जीवन भर दंड कसरत करते रहो। जब, तप, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थाटन, कूप वाटिका बनाना, मंदिर स्थापना इत्यादि का फल स्वर्ग प्राप्ति है।
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।।
(गीता 2-44)
विद्वानों द्वारा जो समय-समय पर इस ओर लक्ष्य कराया जाता है, इस प्रकार का जो उपदेश देते हैं और स्वर्ग दिखाते हैं, उन्हें स्वर्ग का पासपोर्ट दे देते हैं। परन्तु चित्त की आसक्ति को नहीं मिटा सकते। अज्ञानी हृदय कभी भी निष्काम नहीं हो सकता। सुन लो कान खोलकर-अज्ञानी हृदय यदि कामना रहित हो जाए तो बन्ध्या का पुत्र हो सकता है। निराधार आकाश में पुष्प खिल सकते हैं। कछुवे की पीठ पर बाल उग सकते हैं, खरगोश के सींग हो सकते हैं, यह सब होना असंभव है। जब तक निष्काम कर्म नहीं होता तब तक वह कामनासक्त ही है। जो दारासक्त, पुत्रासक्त, वित्तासक्त है, उनके लिए विद्वान लोग सकाम कर्म का उपदेश देते हैं। अरे भाई ! क्यों नहीं-देखो यहाँ पर हम तुम्हें उपदेश दे रहे हैं और तुम सब यही तो मानोगे कि स्वामीजी जो कुछ कह रहे हैं, सब सत्य है। तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम तुम्हें क्या कह रहे हैं, इसकी परख करें। वरन् यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें उचित सत्य का मार्ग निर्देश करें। यह सब विद्वानों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इसीलिए इतना सब श्रम हो रहा है। इसलिए-
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।।
(गीता 2-43)
जिनकी बुद्धि में वासनाओं का जाल बिछा है, कामनाओं से भरपूर हैं, वे इस आत्मतत्व को क्या जानेंगे। ऐसी बुद्धि को व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। वे कोई भी मंदिर में, तीर्थ में, व्रत, दान आदि करते हैं, उनकी बुद्धि में कामना अवश्य रहती है। कामना लेकर ही करते हैं कि हम धनवान हो जाएँ, सुखी रहें, पुत्र हों, बाल बच्चे हों ऐसी कामनासक्त बुद्धि को व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। तो-
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।।
(गीता 2-45)
अर्थात् ऐसे कामनासक्त जीवों की बुद्धि समाधि (आत्मा) में संलग्न नहीं हो सकती। व्यवसायात्मिका बुद्धि वालों को आत्म तत्व का विचार अच्छा नहीं लगता। वे ज्ञान का नाम सुनकर उसमें कीचड़ उछालते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं। ज्ञान से दूर भागते हैं-जी हाँ, मुक्ता को इसका बड़ा अनुभव है, काफी तजुर्बा है। चालीस वर्ष से यही तो हम देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत, श्री रामायण और श्रीमद् भगवद गीता का सदैव हर जगह कार्यक्रम होता रहता है और इसमें शिक्षित वर्ग और अपढ़ भी (जो नहीं पढ़े-लिखे हैं, वे सभी) आते हैं। परन्तु कभी भी भटककर व्यापारी वर्ग-व्यवसायात्मिका बुद्धि वाले नहीं आते, क्या मजाल जो ऐसे वर्ग आ जाएँ। जी हाँ! और यदि कुछ आ भी जाएँ तो यह अपवाद है। भैया ! यह उनका पुण्य है, तप है, कि ऐसों को भी ज्ञान में रुचि है। व्यापारी आयेगा भी तो कुछ न कुछ कामना लेकर ही आएगा। कुछ न कुछ अवश्य मांगेगा। धन, बेटा-बेटी, स्त्री मांगेगा, माया ही मांगेगा, भगवान लेकर क्या करेगा। हाँ-
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।।
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।।
(गीता)
यही व्यवसायात्मिका बुद्धि है और श्रीमद् भागवत में इसी को कूटधम कहते हैं। तो राजा प्राचीनवर्हि भगवान नारद से प्रश्न करता है-
न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः ।
ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः ।।
मूढ़ अज्ञानी पुरुष भगवान आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसका हृदय कामनाओं से भरा रहता है। जिज्ञासुओं! यहाँ पर कर्मों का विवेचन हो रहा है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय क्या है? सुनो-आनंद से सुनो, जो जहाँ बैठे हो। देखो यदि ऐसा कहो कि कर्म से अज्ञान का नाश होता है तो जान लो कि कर्म से अज्ञान का नाश नहीं होता। यह बात निर्विवाद सिद्धांत है। समझो-
सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्य ।।
अर्थात् जो कार्य जिस संबंध से उत्पन्न होता है वह उस संबंध के नाश का कारण नहीं हो सकता। तो कर्मों का मूल कारण अज्ञान है, पुण्य हो या पाप हो, सभी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, अज्ञान से पैदा हुए हैं। जो कर्म अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं वे अज्ञान का नाश किस प्रकार कर सकते हैं। अज्ञान से उत्पन्न कर्म के द्वारा अज्ञान नष्ट नहीं हो सकता।
अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते ।
विद्यद्यैव तन्नाशविधौ पटीयसी न कर्मतज्जं सविरोध मीरितम् ।।
(श्री रामगीता 9)
कर्मों का मूल कारण अज्ञान है तो अज्ञान के नाश में कर्म समर्थ नहीं है। विद्यैव यानी ज्ञान ही अज्ञान का नाश करने में समर्थ है।
छूटइ मल कि मलहि के धोये। घृत कि पाव कोई वारि बिलोये ।।
(उ.का।)
कीचड़ से धोने से मल का नाश नहीं होगा। इसी प्रकार अज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं होगा। मल से मल का नाश संभव नहीं है। सुनो-यहाँ पर हम कर्म के प्रकार और उनसे छूटने का उपाय बताएँगे। कर्म दो प्रकार के होते हैं- पाप कर्म और पुण्य कर्म। वेदों में इसी को धर्म और अधर्म कहते हैं।
वेदप्रणिहितो धर्मोह्यधर्मस्तद्विपर्ययः ।
वेदो नारायणः साक्षात्स्वयम्भूरिति शुश्रुम ।।
(श्रीमद् भागवत 6/1/40)
वेदों में कर्म को धर्म-अधर्म कहते हैं। वेद जिनके लिए आज्ञा देते हैं वह धर्म है और जिसके लिए निषेध करते हैं वह अधर्म है। पुराणों में इसी को पुण्य और पाप कहते हैं तथा धर्मशास्त्र में इसी को शुभ और अशुभ कहते हैं। मतलब सबका एक ही है। अन्तःकरण में जब तक धारणा के रूप में है तब तक उसका नाम धर्म है और जब शरीर द्वारा बहिर्मुख होता है तो धर्म का नाम कर्म पड़ जाता है। तो धर्म का स्थूल रूप कर्म हुआ। पुण्य और पाप के पर्यायवाची धर्म और अधर्म है। वस्तुतः धर्माधर्म की यह व्याख्या तो उनके लिए तो ठीक है जो वेदों, शास्त्रों से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते अथवा जो वेद शास्त्रों को मानते ही नहीं हैं, जो नास्तिक हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए धर्माधर्म की क्या व्याख्या हो? पुण्य-पाप किस धर्म को कहें? नास्तिक तो धर्म क्या, ईश्वर को ही नहीं मानता तो वेदों की आज्ञा को क्यों कर मानेगा। इसमें वर्णित लक्षणों को नहीं मानेगा तो फिर वह कौन-सी व्याख्या हो जो सार्वभौम हो, जिसको सभी मानें, जिसे सब समझ सकें? तो सुनो-जिस कार्य के करने से हृदय में लज्जा और भय न लगे। उस कार्य को धर्म या पुण्य कर्म कहते हैं और जिस कार्य को करने से हृदय में भय, लज्जा लगे वह कर्म अधर्म है, पाप है। बस, यही सार्वभौम सिद्धांत है। अब अपने आप चुन लो, दुनियाँ में कौन भय के और कौन लज्जायुक्त कर्म है। बस, अपने-अपने हृदय पर हाथ रखकर परख लो, हजारों हृदय यहाँ पर बैठे हैं-चुन लो भाई-बस, धर्माधर्म का यही अर्थ है। चलिये आगे। कर्म चार प्रकार के हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और काम्य कर्म। भैया ! कर्मों का बड़ा भारी जाल है। समझना- वेदों के मंत्रों की संख्या एक लाख है। इसमें अस्सी हजार मंत्र सिर्फ कर्मकांड के हैं। सोलह हजार मंत्र उपासना के हैं और शेष चार हजार मंत्र ज्ञान के हैं। लाखों मन रूई के ढेर को जलाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। देखो- यहाँ पर बहुत से ब्राह्मणों का समुदाय बैठा है और सभी यज्ञोपवीत पहनते हैं। जब ब्राह्मण जनेऊ बनाता है तो कितने चौवे का बनाता है? (चौवे- चार अंगुल का) छियान्बे चौवे का। तो भाई ! छियान्बे चौवे ही क्यों? क्यों न एक सौ आठ चौवे के बनाते हो? तो इसका कारण यही है कि वेद मंत्रों के अस्सी हजार मंत्र कर्मकांड के और सोलह हजार मंत्र उपासना कांड के, इससे (80+16) छियान्बे हजार हजार मंत्रों के कारण छियान्बे चौवे का जनेऊ बनता है। ब्राह्मण को इन मंत्रों पर अधिकार है। भाई! हम पढ़े भी हैं और पढ़ाएँ भी हैं। जी हाँ- क्षत्रिय के लिए नब्बे चौवे का जनेऊ बनता है, कारण कुछ मंत्र दान प्रतिग्रह के हैं, वे क्षत्रिय जाति पर लागू नहीं होते। उन्हें दान का अधिकार नहीं है, जिसके कारण नब्बे चौवे का जनेऊ पहनते हैं। वैश्य को पच्यासी और शूद्र को अस्सी चौवे। कहीं-कहीं शूद्र को भी जनेऊ बिना मंत्र के विवाह के समय दे दिया जाता है। उनके लिए अस्सी चौवे का जनेऊ होता है। चलो क्या-क्या कहें- बड़ा भारी जाल है। तो कर्म के चार भेद-नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और काम्य। नित्य कर्म तो जाति वर्ण के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसे ब्राह्मण को उनके वर्ण के अनुसार उनके अधिकार के अनुसार उन्हें संध्या, अग्निहोत्र, मंत्र, जाप, गायत्री आदि नित्य करना चाहिए! ये कर्म नित्य कर्म हैं। इन कर्मों के करने से कोई पुण्य नहीं है। अरे भाई ! जिसका करना तुम्हारा साधारण धर्म है, जो तुम्हें नित्य करना ही चाहिए, तो फिर ऐसे कार्यों को करने से क्या पुण्य, यह तो तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हें करना अनिवार्य है। यह ब्राह्मण की ड्यूटी है। हाँ-यदि न करो तो पाप अवश्य लगेगा। इसलिए जो कर्म तुम्हारे लिए विहित हों उसे करने में पुण्य नहीं, पर न करने से पाप है। दूसरी बात हर एक गृहस्थ चाहे वह राजा हो या भिखारी सभी गृहस्थ के यहाँ पाँच पाप नित्य होते हैं- चक्की में, चूल्हे में, ओखली में, झाडू-बुहारु लगाने में और पाँचवाँ पानी रखने की जगह में। पाँचों जगह जाने-अनजाने जीव हिंसा होती है। तो चाहे कोई गृहस्थ हो अथवा संन्यासी, जिसके यहाँ चूल्हा-चक्की, आडम्बर होगा उसके यहाँ ये पाँच पाप नित्य होंगे। अर्थात् जो साधु, संन्यासी बनते हैं और आश्रम बनाकर रहते हैं तो फिर उनके यहाँ भी तो ये पाँच पाप होते ही हैं। तो गृहस्थ हो या संन्यासी-हाँ इसीलिए तो संन्यासी को कुटी बनाने का निर्देश नहीं है। सिर ढाँकने के लिए चलो कुटी बना लें तो क्या मजाल की चूल्हे का बंदोबस्त न हो। तो चूल्हा-चक्की चाहे साधु के यहाँ हो या गृहस्थ के यहाँ-हम यह सब जानते हैं, यह हमारा अनुभव है कि गृहस्थों की बात क्या कहें-आश्रमधारी साधु कुत्ते को एक टुकड़ा भी नहीं देते, मार भगाते हैं। क्योंकि, साधु तो जानते ही हैं कि वे अब साधु हो गए हैं, अब कुत्तों का क्या काम, वही प्रपंच है वहाँ भी, चाहे गुप्त हो या प्रगट वही बात। हम तो चिल्लाकर कह रहे हैं। यहाँ हमको किसका भय है। अंगूठा रखने की भी जमीन जिसके पास न हो, वृक्ष के नीचे जो रहे वही यह निर्भय होकर कह सकता है। ''महत्पदं ज्ञात्वा वृक्ष मूले वसेत्।" महानपद भगवान आत्मा को प्राप्त करके वृक्ष के नीचे रहना चाहिए। अरे यार ! क्या घर-बार इसीलिए छोड़े हैं? तो फिर क्या घर छोड़कर फिर घर बसावें? यह ठगनी माया बड़ी विचित्र है। गृहस्थी बेचारे तो माया में पिरोये ही हैं, परन्तु यह ठगनी माया साधुओं के पीछे हाथ धोकर पड़ती है-कहती है हमें छोड़कर कहाँ जाओगे। इस माया से बड़ा भय है। इन पाँचों पापों से मुक्त होने के लिए शास्त्रों में पंच बलिवैश्व का विधान है। काग बलि, अग्नि बलि, गो बलि, अतिथि बलि, श्वान बलि। गृहस्थ पाँच मुट्ठी अन्न, आटा, चॉवल इनके लिए निकाल देते हैं। कोई-कोई पाँच ग्रास निकाल देते हैं। यह नित्य कर्म है। प्रश्न होता है यदि ऐसा न करे तो? तो भैया! ब्याज सहित अपना-अपना भाग ले लेंगे। घर में कोई बीमार हुआ तो हजारों निकल जाएगा, तुम्हारा ब्रह्मपना निकल जाएगा। इसलिए जिस आश्रम में रहना, उसका पालन करना चाहिए।
सोचिय गृही जो मोहबस करइ करम पथ त्याग ।
सोचिय यति प्रपंचरत विगत विवेक विराग ।।
'न सुखं न दुःखं, न पुण्यं न पापं शिवोऽहम् शिवोऽहम्'-इससे काम न चलेगा। यह तुम्हारी ड्यूटी है और इसका पालन तुम्हें करना ही होगा।
तीर्थ, व्रत, दान इत्यादि कर्म जब सूर्य लोक, चन्द्रलोक एवं स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त किए जाएँ तो उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। ये ही कर्म जब स्त्री, पुत्र, धन आदि की कामना से किये जाए तो उसे काम्य कर्म कहते हैं। यही कर्म जब पापों से छुटकारा पाने के लिए किये जाएँ तो उसे प्रायश्चित कर्म कहते हैं। तो कर्म चार प्रकार के-नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और काम्य। अब कर्मों के भेद सुनो- कर्म तीन प्रकार के संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इनके शब्दार्थ पहिले समझ लो। संचित कर्म-जो जन्म जन्मांतर से एकत्रित हुआ हो। प्रारब्ध कर्म-जो ऊपर जमा हुआ कर्म उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया। क्रियमाण कर्म-निकले हुए हिस्से से कुछ कर्म कर्ज में दे दिया। इसे पहले दृष्टान्त से समझो, बाद में इसको भाव रूप में घटा लेना। तुम्हारे मकान के अंदर गल्ला रखने का एक ऐसा स्थान बना होता है जिसे खत्ती, ढाबा अथवा बंडा कहते हैं। इस खत्ती में तुम हजारों मन गल्ला रखते हो। ध्यान दो-उस खत्ती में साल-साल भर के बचत अन्न, मोटा, पतला, महीन, नया-पुराना सभी किस्म का अन्न (गल्ला) कई वर्षों का भरा पड़ा है। इसकी कोई तादाद नहीं है। इस खत्ती में कितना अन्न मोटा, कितना महीन, कब-कब का पुराना नया सभी भरा है, इसकी तादाद नहीं है। बस यही संचित है। अब इसमें से कुछ निकाल लिया, उसमें मोटा, महीन, पुराना, नया सभी मिला हुआ है। यही प्रारब्ध होगा। अब उस निकले हुए अन्न से कुछ तुमने ब्याज में किसी को दिया, सवाया या डेढ़ी। जब लोग एक मन अन्न ले जाते हैं तो लुवाई के बाद सवा मन या डेढ़ मन वापस देते हैं। तो यहाँ पर क्या लेते हैं। सवाया। चलो भाई! कुछ तो ईमानदारी है। कहीं-कहीं डेढ़ी वसूल करते हैं। अब यदि कर्जदार साल भर में ब्याज पटा दे तो ठीक है, नहीं तो यदि वह न दे सके तो साल भर में साहूकार उस ब्याज को भी मूल धन में शामिल करके उसके ऊपर भी अगले वर्ष ब्याज लेता है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कर्ज देने वाला ऋणी को बुलाकर हिसाब करता है और उसे बताकर ब्याज को भी मूल में मिला देता है। तो भैया ! यह चक्रवृद्धि पानी सरीखे बढ़ता है। बड़ी-बड़ी रियासतें बिक जाती हैं। घर- बार सब बिक जाता है। तो जो ब्याज का अन्न आया वह भी उसी खत्ती में डाल दिया गया यह खत्ती इतनी विशाल है कि कभी भरती ही नहीं, सदैव खाली ही रहती है।
आगे अब दृष्टांत का द्राष्टांत समझो। मतलब यह है कि यह साढ़े तीन हाथ का शरीर ही मकान है। इसके भीतर ही खत्ती है। उसका नाम मन है, तो मन नाम की खत्ती है। एक जन्म और अनेक जन्मों के पाप-पुण्य कर्म अनादिकाल से मन रूपी खत्ती में भरे पड़े हैं। यही संचित कर्म है। जब कोई शरीर धारण किया तो इसी संचित कर्म से कुछ पुण्य-पाप कर्म को लेकर वह जन्म धारण करता है। इस जन्म के ये ही प्रारब्ध कर्म हुए। इसको प्रारब्ध कर्म कहो चाहे शरीर कहो दोनों का मतलब एक ही होता है। इस साढ़े तीन हाथ के शरीर द्वारा इस समय जो पुण्य-पाप कर्म हो रहे हैं, उन्हें क्रियामाण कर्म कहते हैं। ठीक-
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।।
(गीता 3/27)
इन कर्मों का कर्ता, भोक्ता मैं हूँ ऐसा जो अहंकार यही चक्रवृद्धि ब्याज है। इसी कारण जीव कर्म बंधन में स्वयं पड़ा है। तो यह कर्मजाल बड़ा भयाक है। सब गड़बड़-सड़बड़ है। भैया ! इस कर्मजाल से से निकलना चाहो तो तुम भी वही करो जो हम किए हैं। इस कर्म रूपी खत्ती में आग लगा दो, फूँक से और ब्याज लेना बंद करो। इस कर्म जाल से बचना चाहते हो तो हम बता रहे हैं-इस खत्ती को जला दो और ब्याज लेना बंद करो। इधर पूंजी भी खतम और आमदनी भी बंद। तो फिर दिवालिया हो जाएगा। हाँ भाई ! दिवालिया तो बना ही रहे हैं। रह गया यह साढ़े तीन हाथ का शरीर-प्रारब्ध कर्म। जब सभी खतम हो गए तो फिर यह भी कब तक चलने वाला है। इसलिए अपना घर फूँक दो। ऐसा क्यों? क्योंकि, जो अपना घर फूंका होगा वही ऐसा कहेगा। घर फूंकने की कला सबको थोड़े ही आती है।
कबीरा खड़ा बाजार में लिये लुवाठी हाथ ।
जो घर फूँकै आपनो चलै हमारे साथ ।।
लुवाठी कहते हैं अधजली लकड़ी को। तो तैयार हो जाओ, जिसको हमारे साथ चलना है। आगे आओ-आग जो लगाना है। गीता भी श्री योगेश्वर भगवान का वचन है-
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् ।
पश्यशृणवन्स्पृशञ्जिघ्घ्रन्नश्रनाच्छन्स्पश्वसन् ।।
(गीता 5-8)
तत्ववेत्ता पुरुष ऐसा मानता है कि 'अहम् किञ्चत् न करोमि ।' मैं कर्मों का कर्ता-भोक्ता नहीं हूँ। यह मान्यता क्या समझकर करता है? इस तरह किस सिद्धांत से मानता है?
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।।
(गीता 13-31)
यह निर्विवाद सिद्धांत है कि कर्म बंधन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। मैं आत्मा हूँ, अनादि हूँ-जन्म का पता ही नहीं, सत, रज, तम से परे हूँ। मैं अव्यय-अविनाशी हूँ, शरीर के अंदर रहते हुए भी मैं कर्मों का कर्ता-भोक्ता नहीं हूँ। न लिप्यते, इस तरह मानकर कर्म के जाल में लिप्त नहीं होता, क्योंकि 'मैं' साक्षी हूँ।
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।।
(श्वेता 6-11)
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमियं रविः ।
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ।।
(गीता 13-33)
सूर्य अनेकानेक ब्रह्माण्डों में एक-सा प्रकाशित हो रहा है और जैसे इस स्थान में इसी प्रकाश में यहाँ ब्रह्म निरूपण हो रहा है, उसी तरह इसी प्रकाश में अन्यत्र घोर से घोर पाप भी हो रहा होगा-तो यहाँ का पुण्य और कहीं का घोर पाप जैसे सूर्य में नहीं होता, सूर्य में कर्ता-भोक्ता का भाव नहीं होता, सूर्य पर इस प्रकार का आरोप नहीं लग सकता चाहे जहाँ पुण्य या पाप हो। इसी प्रकार 'मैं' आत्मा पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान इन सब में एक रस प्रकाशित हूँ, इनको जानता हूँ। यद्यपि इनके व्यापार हो रहे हैं और 'मैं' आत्मा के साक्षित्व में हो रहे हैं, परन्तु 'मैं' पर ये आरोपित नहीं हो सकते। 'मैं' वास्तव में इन सब का ज्ञाता हूँ। 'मैं' के साक्षित्व में ही कार्य हो रहे हैं, परन्तु 'मैं' में कर्मों का कर्तापना नहीं है। 'मैं' साक्षी हूँ। साक्षी के तीन लक्षण- द्रष्टापना, ज्ञातापना और नजदीकपना। कोर्ट में जब न्यायाधीश पूछता है कि तुमने अमुक को अमुक के सिर पर लाठी मारते देखा है? गवाह कहता है- हाँ सरकार ! मैंने देखा है तो द्रष्टापना हुआ तुम जानते हो इसकी लाठी लगी है। हाँ सरकार! मैं जानता हूँ कि इसी की लाठी लगी है। यह ज्ञातापना हुआ और जब उसने लाठी मारी तो तुम कहाँ पर थे? साहब ! मैं उस समय बहुत करीब था। तो यह हुआ नजदीकपना। इस प्रकार का जो साक्षी है उसके ही बयान पर अदालत फैसला देती है। तो साक्षी स्वयं अक्रिय होता है, निर्दोष होता है, निष्कलंङ्क होता है, तटस्थ होता है। इसी तरह 'मैं' आत्मा साक्षी हूँ। मेरा मन अच्छे में जाता है या बुरे में जाता है, स्थिर होता है अथवा चंचल होता है, दुःखी या सुखी होता है, निर्विकार या सविकार होता है, इत्यादि भावों को 'मैं' आत्मा जानता हूँ। यथा प्रमाण-
अहं साक्षीति यो विद्यात् विवित्तयैवं पुनः पुनः ।
स एव मुक्तः स विद्वान इति वेदांत डिमडिमः ।।
कोई ऐसा टाईम नहीं कि मुझसे चोरी करके मेरा मन भले या बुरे में चला जाए। 'मैं' दिन-रात देखता रहता हूँ। मन के सारे व्यापारों (चेष्टाओं) को 'मैं' जानता हूँ और मन से 'मैं' इतना नजदीक हूँ कि 'मैं' स्वयं मन हूँ। हाँ, इतना नजदीक हूँ कि जिसको 'मैं' जानता हूँ, वही होकर जानता हूँ। तो मन का ज्ञाता, मन का द्रष्टा और नजदीक स्वयं 'मैं' ही मन हूँ। इसलिए 'मैं' मन का साक्षी हूँ।
देखो-ध्यान दो। जरा फारमूला बता दूँ-द्रष्टा जब दृश्य को देखता है, तो दृश्य के दर्शनकाल में दृश्य से भिन्न होकर देखता है या अभिन्न होकर अभिन्न होकर देखता है। देखो ऐसा कहने से हम नहीं मान लेंगे। बाप का नाम बताओ नहीं तो श्राद्ध करो। दृश्य के अनुभवकाल में द्रष्टा दृश्य से भिन्न होकर यदि देखे तो दृश्य नहीं और यदि दृश्य से अभिन्न होकरदेखे तो भी दृश्य नहीं और यदि द्रष्टा दृश्य से भिन्न है तो दृश्य नहीं अभिन्न है तो भी दृश्य नहीं। सब अनुभव करो इसको-जैसे डंडा है, यह दृश्य है बिल्कुल उसी टाईम यानी दर्शनकाल में? इसलिए 'मैं' आत्मा जिसको देखता हूँ, जिसको जानता हूँ, वही होकर देखता, जानता हूँ। तो वस्तुतः यदि कुछ द्रष्टा से दृश्य भिन्न हो तो अलग-अलग अनुभव हो, परन्तु ऐसा नहीं होता इसलिए जिसका 'मैं' अनुभव करता हूँ, वही होकर अनुभव करता हूँ।
समुझि सयाने करहु अब, सब मिलि संमत सोई ।।
(रा. अयो.)
क्या मतलब? जी हाँ, द्रष्टा होकर दृश्य का अनुभव नहीं होता, परन्तु द्रष्टय दृश्य एक होकर ही अनुभव होता है। तो द्रष्टा कहाँ गया और द्रष्टा ही नहीं, तो उसकी अपेक्षा से ही तो दृश्य था, अतः दृश्य भी नहीं और द्रष्टा दृश्य नहीं तो दर्शन किया कहाँ। बस, चेतन का चेतन तत्व रह गया 'मैं' का 'मैं'। अरे! क्या यहाँ भी झगड़ा है? अभी अनुभव करो तुम्हें कुछ बुद्धि द्वारा या तर्क द्वारा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर तो स्वरूप का कथन हो रहा है। जिसको देखते जानते हो, वही होकर देखते जानते हो या भिन्न-भिन्न होकर देखते जानते हो? जिसको जो देखता है वही होकर उसको देखता है। यहाँ तो नकद सौदा है। अनुभव यहीं पर कर लो। कोई उधार बात नहीं है। मजा आ गया।
इसलिए 'मैं' सर्व का साक्षी हूँ, अतः अक्रिय हूँ। साक्षी में कर्तापना, भोक्तापना नहीं होता। तो 'मैं' साक्षी भाव से सदैव सर्वदा सब के हृदय में विराजमान हूँ। अच्छा, तो फिर उस मन रूपी खत्ती में जो कर्मों का भंडार है उसमें आग लगा देनी चाहिए। तो लो यह आग लगा दो-कर्ता, भोक्ता अपने आप में अज्ञान से ही माना था। 'मैं' कर्ता, भोक्ता भूतकाल में भी नहीं था, 'मैं' कर्ता, भोक्ता अब भी नहीं हूँ और कर्ता, भोक्ता भविष्य में भी नहीं रहूँगा। इस तरह जब कर्ता, भोक्ता नहीं तो कर्तापने के अहंभाव का नाश हो गया। केवल साक्षी मात्र रह गया। अहंभाव के नाश होते ही पूंजी खत्म। खत्ती में आग लग गई। आज भी मैं कर्ता नहीं हूँ, ब्याज भी गया। क्रियमाण कर्म का नाश हो गया। तो इस तरह पूंजी भी गई और उसका बढ़ता ब्याज भी चला गया। आमदनी बंद हो गई। रह गया साढ़े तीन हाथ का शरीर- प्रारब्ध। कई विद्वान प्रारब्ध का नाश नहीं मानते- ऐसा मानने से गुरु परम्परा की हानि होती है। वे ऐसा समझते हैं कि ज्ञान से संचित और क्रियमाण का नाश होता है, परन्तु प्रारब्ध का नहीं। तो भाई ! क्योंकर प्रारब्ध का नाश नहीं होता? यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रारब्ध भी अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इसका भी मूल कारण अज्ञान ही है। जब तीनों कर्मों का मूल कारण अज्ञान है तो प्रारब्ध क्यों नहीं जला, अज्ञान रूपी प्रारब्ध कैसे रह गया। बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी प्रारब्ध का शेष रह जाना मानते हैं। जब संचित क्रियमाण एवं प्रारब्ध सभी का मूल कारण अज्ञान है और जब अज्ञान का नाश हो गया तो प्रारब्ध क्यों कर शेष रह जाएगा? क्या कारण है। तो यहाँ पर बड़े-बड़े आचार्य बैठे हैं उनसे पूछो-यहाँ पर तो बहुत सीना फुलाए बैठे हैं बतावे क्यों प्रारब्ध बच रहता है? तो उनकी यही एकमात्र दलील है कि भाई! देहधारी गुरु से ही बोध होता है। तो प्रारब्ध का नाश मानने से गुरु परम्परा का नाश हो जाएगा। देह भाव रहते गुरु शिष्य संबंध को कैसे लोप करें तो इस तरह आँसू पोंछते हैं। यह कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। सुनो-भगवान श्री कृष्ण सीधे तो है नहीं, सदैव टेढ़ा रूप बनाते हैं। तो उनका कहना भी टेढ़ा ही होगा, कैसे जल्दी लगे-
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित् ।
पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्नन्नश्ननगच्छन्स्वपश्वसन् ।।
(5 - 8)
प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ।।
(5-9)
मैं कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।
(गीता 5-10)
इस प्रकार मैं कर्मों का कर्ता, भोक्ता नहीं हूँ। अज्ञान के कारण ही लोग अपने आपको कर्ता, भोक्ता मान लेते हैं। परन्तु संसार में ऐसे रहना चाहिए जैसे पद्मपत्रमिवाम्भसा। पानी में रहते हुए भी कमल का पत्र पानी से अलग रहता है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान प्रारब्ध को मानते हैं। इस कथन द्वारा प्रारब्ध का शेष रहना माना है। अच्चा चलो आगे चलें।
यथैधांसि समिद्धोऽग्रिर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।।
(गीता 4-37)
वाह रे कन्हैया ! जैसा तू है वैसा ही तेरा कथन है। अब इसको मानें कि उसको मानें? एक जगह भगवान प्रारब्ध का शेष रहना कहते हैं और एक जगह सभी कर्मों को प्रारब्ध सहित भस्मसात् करते हैं। किस अभिप्राय से? भगवान प्रारब्ध को शेष रहना आचार्य देश से मानते हैं और ज्ञानाग्नि से सर्व कर्मों का भस्म हो जाना भगवान देश से मानते हैं। भगवान वहाँ, पर-देश से बोल रहे हैं और भगवान यहाँ, स्व-देश से बोल रहे हैं। ज्ञान से समस्त कर्मों का भस्म होना स्व-देश की बात है और प्रारब्ध का नाश न होना यह पर-देश की बात है। तो पर-देश और स्व-देश क्या है? मजा लो-
नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित् ।।
'तत्ववित् इत्येवं मन्येत न तु विजानीयात् 1' तत्ववित् (तत्ववेत्ता पुरुष) ऐसा मानता है कि तत्ववित् ऐसा जानता है। अहं ब्रह्मास्मि की धारणा वाले को
तत्ववेत्ता कहते हैं। अहमस्मि इस निश्चय वाले को आत्मनैष्ठिक कहते हैं यानी आचार्य देश में अहं ब्रह्मास्मि की धारणा होती है और भगवान देश में अहमस्मि का निश्चय होता है। देखो, तीन प्रकार का अध्यास होता है। यहाँ पर बड़े-बड़े वेदांत ग्रन्थ को निगल कर बैठे हैं। समझो विषय-यहाँ विद्वान लुधियाना, दिल्ली आदि स्थानों से आए हुए एकत्रित बैठे हैं। कान खोलकर सुन लो- अध्यास तीन प्रकार का होता है। क्यों भाई ! चार प्रकार का क्यों नहीं होता? क्योंकि गुण भी तो तीन प्रकार के होते हैं-सत, रज, तम। अच्छा, हाँ जी- देहाध्यास, जीवाध्यास और ब्रह्माध्यास। मैं देह हूँ-यह देहाध्यास है और तमोगुणजन्य है। मैं जीव हूँ, ऐसा मानना, जीवाध्यास रजोगुणजन्य है और मैं ब्रह्म हूँ, यह ब्रह्माध्यास सतोगुणजन्य है। बिल्कुल ठीक-जब 'मैं' को तीनों से हटा लो- 'मैं' आत्मा में देह का अध्यास 'मैं' में जीव का अध्यास और 'मैं' में ब्रह्म का अध्यास, तो ये तीनों अध्यास किस पर आधारित हैं? 'मैं' पर। तो तीनों का आधार 'मैं' आत्मा ही हूँ। मैं देह हूँ-यह अध्यास मैंने माना। मैं जीव हूँ-यह अध्यास मैंने माना। 'मैं' ब्रह्म हूँ-यह भी अध्यास मैंने ही माना। इसीलिए तो भगवान कहते हैं 'मन्येत'। अरें! 'मैं' पर से जीव भाव को हटाने के लिए ही तो 'मैं' ब्रह्म हूँ - यह धारणा की गई। जीव भाव का अभाव करने के लिए 'मैं' ब्रह्म हूँ-यह धारणा बनाई गई।
सर्व व्यापारमुत्सृज्य अहं ब्रह्मेति भावय ।
अहं ब्रह्मेति निश्चित्य त्वहंभावं परित्यजेत् ।।
विशेष दर्शिनिः आत्मभाव भावना विनिवृत्तिः ।।
(यो.द.कै. पाद)
भगवान वेद व्यास स्कन्धपुराण के 21वें अध्याय में कहते हैं-
अच्युतोऽहं अनन्तोऽहं गोविंदोऽहं अहं हरिः ।
आनन्दोऽहं अशेषोऽहं अजोऽहं अमृतोस्म्यहम् ।।
नित्योऽहं निर्विकल्पोऽहं निराकारोऽहमव्ययः ।
सच्चिदानंद रूपोऽहं परिपूर्णोऽस्मि सर्वदा ।।
ब्रह्मैवाहं न संसारी मुक्तोऽहं इति भावयेत् ।
मैं अच्युत हूँ, मैं अनन्त हूँ, मैं गोविंद हूँ, मैं आनंदस्वरूप हूँ, मैं व्यापक हूँ, चैतन्य घनभूत हूँ ऐसा अपने आप में भावना करें। इति भावयेत् 'मैं' पर ऐसी भावना करे। यहाँ पर जानना नहीं कहा। देह भाव, जीव भाव को हटाकर इस प्रकार की भावना करे। भावना तो हमेशा कल्पित होती है। अहं ब्रह्मास्मि-यह भावना है। मैं ब्रह्म हूँ-यह ज्ञान माना हुआ है। कल्पित ज्ञान है। आचार्य द्वारा प्रतिपादित 'तत्वमसि' महावाक्य के श्रवण, मनन, निदिध्यासन से वृत्ति में उदय हुआ। जो ज्ञान, जिसे अहं ब्रह्मास्मि की धारणा (भावना) कहते हैं। क्षणिक ज्ञान, विशेष ज्ञान, असत्य ज्ञान, अनित्य ज्ञान, नश्वर ज्ञान, इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। यह बोध नहीं है। यदि तुम्हारी यही धारणा है तो इसे निकाल दो। आगे भी यदि यही धारणा रही तो पूर्ण बोध नहीं है, बल्कि भावनात्मक बोध है। पहले अपने आपको जीव मानते थे और अब अपने आपको ब्रह्म मानते हो। हाँ, पहले गरीब थे और अब कुछ अमीर बन गए। तो यह छोटा अभिमान और यह बड़ा अभिमान, यही अंतर रहा। परन्तु, मिला क्या? खाक। क्या इसी को ज्ञान कहोगे? इस तरह की मान्यता ने ही सब बरबाद कर दिया है। यहाँ पर अध्यास का प्रतिपादन नहीं हो रहा है। आत्म तत्व का निरूपण हो रहा है। तो ये अध्यास किस प्रकार आधारित है।
इनका आधार क्या है? देखो-तीन प्रकार के वादी होते हैं।
मैं देह हूँ-यह देहात्मवाद है-कर्मकांड का विवेचन करते हैं।
मैं जीव हूँ-यह जीवात्मवाद है-उपासना का विवेचन करते हैं।
मैं ब्रह्म हूँ-यह ब्रह्मात्मवाद है-ज्ञान कांड का विवेचन करते हैं।
यह द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद। इस तरह ये तीनों वादी छँट जाते हैं। यहाँ कोई वाद नहीं है। यह निर्विवाद है। ऊपर के तीनों वाद निर्विवाद सिद्धांत नहीं हैं। कर्मवादी, कर्मकांडी अपने को मैं हूँ, कहता है। उपासक भी अपने को 'मैं' हूँ, कहता है। और ब्रह्मवादी ज्ञानी भी अपने को 'मैं' हूँ कहता है। तो फिर यदि शुद्ध तत्व 'मैं' आत्मा नहीं तो इन तीनों वादों का आधार क्या होगा? अनुभव करो-इस चीज को समझो भगवान पतञ्जलि योग दर्शन के कैवल्यपाद में सूत्र लिखते हैं- 'विशेषदर्शिनिः आत्मभाव भावना विनिवृत्तिः ।।' पूर्ण रूप से स्वरूप ज्ञान होने पर, आत्म बोध प्राप्त होने पर आत्म भाव की भावना की निवृत्ति हो जाती है। आत्मभाव की भावना क्या है?
अच्युतोऽहं अनन्तोऽहं गोविंदोऽहं अहं हरिः ।
आनन्दोऽहं अशेषोऽहं अजोऽहं अमृतोस्म्यहम् ।।
नित्योऽहं निर्विकल्पोऽहं निराकारोऽहमव्ययः ।
सच्चिदानंद रूपोऽहं परिपूर्णोऽस्मि सर्वदा ।।
ब्रह्मैवाहं न संसारी मुक्तोऽहं इति भावयेत् ।
आत्मबोध होने पर इस आत्मभाव की भावना की निवृत्ति हो जाती है। शुद्ध तत्व रह जाता है। समझो विषय-
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मातकुरुते तथा ।।
(गीता 4-37)
जिस समय पूर्ण रूप से आत्म तत्व का बोध हो जाता है तब संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। देखो आत्मदेश के अज्ञान में शरीरादिक प्रपंच हैं ! जब शरीर ही नहीं तो शरीर से भिन्न वस्तु तो कर्म है नहीं, तो फिर प्रारब्ध कहाँ रहेगा? जब तक अज्ञान का नाश न होगा तभी तक प्रारब्ध रहेगा और यदि अज्ञान का नाश हो गया और फिर भई प्रारब्ध का अस्तित्व मानते हो तो समझ लो कि अभी अज्ञान का समूल नाश नहीं हुआ है। आत्म तत्व के बोध में सभी भावनाओं की निवृत्ति हो जाती है और यही कृतकृत्य पद है। जीव यहाँ पर कृतकृत्य हो जाता है। जिज्ञासुओं ! समझना जरा, यहाँ पर बड़े-बड़े रामायणी बैठे हैं-जिंदगी बीत गई रामायण का पाठ करते-करते- उत्तर कांड के ज्ञान दीपक का प्रसङ्ग देखो ध्यान देना-सुनो-
एहि विधि लेसै दीप तेज रासि विज्ञानमय ।
जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब ।।
जब ज्ञान दीपक जला तो उसकी शिखा क्या है?
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीप शिखा सोइ परम प्रचंडा ।।
अहं ब्रह्मास्मि-यह दीप शिखा है। जब यह साधनजन्य ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसके प्रकाश में-
आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल भेद भ्रम नाशा ।।
प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटै अपारा ।।
सब कुछ हो गया। मानस प्रेमियों! फिर उसी प्रकाश में-
तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। उर गृह बैठि ग्रन्थि निरुआरा ।।
जब यहाँ पर मानसकार कहते हैं कि प्रकाशमय बुद्धि हृदयदेश में बैठकर ग्रन्थि खोलती है। अब मानस प्रेमियों से यह प्रश्न है कि जब प्रबल अविद्या का परिवार नष्ट हो गया तब फिर वह कौन-सी ग्रंथि बच गई जिसको खोलने के लिए बुद्धि ज्ञान के प्रकाश में हृदय देश में बैठकर प्रयत्न करती है। वह कौन- सी ग्रंथि को खोलती है? जिंदगी बरबाद हो गई पाठ करते-करते, परन्तु कभी सोचा भी कि कौन-सी ग्रन्थि बुद्धि को खोलनी बाकी रही? अब शेष क्या रह गया?
तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। उर गृह बैठि ग्रन्थि निरुआरा ।।
छोरत ग्रन्थि पाव जौ सोई। तब यह जीव कृतारथ होई ।।
और जिसके खुलने से जीव कृतार्थ हो जाता है और आगे चलिये-
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया। विघ्न अनेक करइ तब माया ।।
तो फिर माया को क्या पड़ी है जो विघ्न कर रही है? और हाँ-माया कौन सा विघ्न करती है?
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई ! बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई ।।
माया को उजाड़ा जा रहा है। जो विघ्न करती है, आगे बतावेंगे। अभी प्रसङ्ग पढ़ दें-
कल बल छल करि जाहिं समीपा। अंचल बात बुझावहिं दीपा ।।
होइ बुद्धि जो परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ।।
इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना। जहं तहं सुर बैठे करिथाना ।।
आवत देखहिं विषय बयारी। ते हठि देहिं कपाट उघारी ।।
जब सो प्रभञ्जन उरगृह जाई। तबहिं दीप विग्यान बुझाई ।।
ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकाशा। बुद्धि विकल भई विषय बतासा ।।
तब फिर जीव विविध विधि पावई संसृति क्लेश ।।
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई विहगेश ।।
सुनो-अब यह शंका होती है कि वह कौन-सी ग्रन्थि बाकी रह गई है जिसको बुद्धि हृदयस्थान में ज्ञान के प्रकाश में खोलने बैठी है। ज्ञान के लाइट में क्या खोलने बैठती है? सोऽहमस्मि-सोऽहम् तक भी कुछ न कुछ अहंकार बाकी है। अज्ञान कुछ न कुछ बाकी रह गया है, वह ब्रह्म मैं हूँ-इस प्रकाश में कुछ ग्रन्थि हैं, अंधकार है। अब प्रश्न होता है कि जिस ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है वह सत्य है कि असत्य? यदि कहो कि वह ज्ञान सत्य है तो एक तो ज्ञान सत्य है और दूसरा ब्रह्म सत्य, तो वेदांत का द्वैतापत्ति दोष आ जाएगा। सत्य एक ही होता है, दो नहीं। तो ब्रह्म और ज्ञान दोनों सत्य नहीं हो सकते। यदि असत्य कहें तो असत्य तो बन्ध्या का पुत्र होता है, वह है ही नहीं। तो असत्य से असत्य की निवृत्ति कैसे होगी? यदि असत्य से असत्य की निवृत्ति होती है तो प्रमाण दो। तो प्रमाण देते हैं कि स्वप्न में किसी को जंगल में शेर मिला तो उस स्वप्न के शेर को मारने के लिए क्या जाग्रत अवस्था की गोली बंदूक की आवश्यकता है? क्या जाग्रत की बंदूक से स्वप्न का शेर मरेगा? वह तो स्वप्न के ही बंदूक से मरेगा। इसी तरह असत्य से असत्य की निवृत्ति हो जाती है, तो पूर्वपक्षी कहता है कि इस तरह स्वप्न के आधार से असत्य की निवृत्ति असत्य से तो हो जाती है, यह मान लिए, परन्तु श्रीमान् जी इस तरह से अज्ञान भी असत्य और उसका नाशक ज्ञान भी असत्य हो जाएगा और फिर इस असत्य ज्ञान से तुमने जाना किसको? सत्य को जाना कि असत्य को? यदि कहो सत्य को जाना तो असत्य से सत्य का ज्ञान कैसे हो सकेगा? वह भी तो असत्य ही हुआ।
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।
योनस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ।।
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।
अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविजानताम् ।।
(केनोपनिषत् 2-3)
जो कहता है मैंने ब्रह्म को जाना, उसने नहीं जाना और जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना उसने भी नहीं जाना। आप अभी अनुभव कर लो, जिस ब्रह्म को जाना उसे भिन्न करके जाना या अभिन्न करके ? यदि भिन्न करके जाना तो ब्रह्म नहीं और अभिन्न करके जाना तो जाना किसको? और जिस ब्रह्म को जानने की इच्छा करता है वह भिन्न है तो ब्रह्म नहीं और अभिन्न है तो जानेगा किसको? यही अविद्या की ग्रन्थि है। इसी ग्रन्थि को खोलने के लिए अहं ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि हृदय देश में बैठती है। यह ग्रन्थि खुल गई तो जीव कृतार्थ हो जाता है। ग्रन्थि क्या है कि मैं पहले अज्ञानी था अब ज्ञानी हुआ मैं पहिले बद्ध था अब मुक्त हुआ। मैं पहिले जीव था, अब ब्रह्म हुआ। यह ठगनी माया इस समय बड़ों-बड़ों को विघ्न करती है। कहती है- यह देखो तो मेरा स्वामी (मायापति) बनने जा रहा है। जब तक ग्रन्थि नहीं खुली तब तक तो वह माया ही उसका स्वामी है और जहाँ उसको बोध हुआ तो वह अलग हो गया। वह मायापति हो गया। क्योंकि, ग्रन्थि खुलने से वह शुद्ध तत्व 'मैं' का 'मैं' भगवान आत्मा रह जाता है। तो-
शिव विरंचि कहं मोहई को है बपुरा आन।
अस जिय जानि भजहिं मुनि मायापति भगवान ।।
जी हाँ-
यथैधांसि समिद्धौऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसातकुरुते तथा ।।
(गीता 4/37)
यही ज्ञान का स्वरूप है और यही विमल ज्ञान है। इन मर्मों को ठीक तरह से जान लिए बिना बंधन नहीं छूटेगा। जब तक प्रारब्ध का अस्तित्व मान रहे हो तब तक अज्ञान बना हुआ है। जब तक अपने आप को मान रहे हो कि मैं ब्रह्म हूँ तो अज्ञान कहाँ गया है? ठीक, श्रीमान् जी ! अहं ब्रह्मास्मि से क्या समझे कि मैं देह नहीं, मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। यह समझा हूँ-तो बताओ तुम अपने को देह नहीं मानते, परन्तु देह अपने देश में है तो सही, कहीं न कहीं तो देह है, चाहे मैं भले अपने को देह न समझें। देह की अपेक्षा से ही तो आप अपने को ब्रह्म मान बैठे हो, फिर भी अभिमान करते हो कि मैं ब्रह्म हूँ। तो श्रीमान् जी! क्या समझे-देह नहीं हूँ मैं ब्रह्म हूँ। देह तुम नहीं हो, परन्तु देह अपने देश में तो है ही और जब तक देह है तब तक देह का अस्तित्व तो रहेगा ही, यह अमिट सिद्धांत है। अज्ञान के अस्तित्व में ही देह है तो तुम्हारा अलग होने से, इससे क्या बिगड़ना है-इसलिए आगे बढ़ो और संत कृपाका भिखारी बनो। ज्ञान पढ़ने से नहीं होता। आत्म तत्व का जानना साधनजन्य नहीं यह तो कृपाजन्य है। हाँ-वेदों, शास्त्रों का ज्ञान साधनजन्य है, परन्तु भगवान अपना आप, क्या साधन से मिलेगा? हाँ- मैं ब्रह्म हूँ यहाँ तक जीव भाव से परे हुए। पहिले जीवभाव में गरीब थे, अब कुछ अमीर बन गए। हाँ भाई ! गरीब ही अमीर बनना चाहता है। तो क्या टेटकू घसीटू कहीं ब्रह्म बनेगा? मैं जीव हूँ, इस जीवभाव की अपेक्षा से ही तो मैं ब्रह्म हूँ, अमीर बन गए। पहिले अपने को गरीब समझता था और अब भावना करता है कि हम बड़े आदमी हैं। दरअसल जो ब्रह्म है वह क्यों कहता फिरेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। देखो, हम उसको भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि, वह अपने आप को भगवान भी नहीं कहता। भगवान अपने आप को भगवान भी नहीं मानता। भगवान, परमात्मा, ब्रह्म यह नाम तो उपासकों ने रखा है। परमात्मा, अपने आपको भगवान थोड़े ही कहता है। तो फिर तुम क्यों अकड़ते हो-अहं ब्रह्मास्मि कहकर। इससे साफ मालूम होता है कि तुम्हारी कंगाली अभी नहीं गई है। जरा रोशनी में आओ। वाह- फिर भगवान गीता में कहते हैं-
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ।।
(गीता 4 - 19)
क्या मतलब - रामाश्रय से, गोविन्दाय नमो नमः, जो है सो-अरे, जिसने समारम्भाः माइने सब समय निःसंकल्प है, जिसके मन में कोई संकल्प- विकल्प नहीं। विकल्प के बाद ही तो मनीराम की फैक्टरी चालू हो जाती है और जब मन निःसंकल्प है तो फिर मनीराम की फैक्टरी चालू नहीं होगी। यानी में देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म आदि भावनाएँ नहीं होंगी। इन भावनाओं का विकल्प 'मैं' के ऊपर होता है। जब भावनारहित हुआ, योगमाया का पर्दा फाड़कर बाहर फेंक दिया, योग माया का पर्दा उठ गया-अरे ! वाह रे यार ! खूब पर्दानशी है, बुरकावाली है, बुरका वाली सभी को देखती है, परन्तु दुनियाँ उसको नहीं देख पाती। योगमाया के परदे में छुपा हुआ 'मैं' आत्मा सबको देखता हूँ, इन्द्रियों को, मन को, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि को, परन्तु सब मुझे देखने में समर्थ नहीं है। वाह-
यह खेल कैसा परदानशीं का, परदा उठाकर जो हमने देखा ।।
इस पद का भाव, अभी नहीं इस वक्त नहीं, उस वक्त सुनाएँगे आत्मजिज्ञासुओं ! ज्ञानाग्नि में सर्व कर्म-संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण सभी भस्म हो जाते हैं। यह भगवान अपने स्वरूप से बोल रहे हैं, अपने देश से कह रहे हैं और प्रारब्ध का रह जाना आचार्य देश से कहे हैं। इस प्रकार भगवान नारद राजा प्राचीनबहिं के प्रति विमल ज्ञान का उपदेश कर्मों के विषय में कर रहे हैं।
---------
द्वितीय दिवस : दूसरी बेला
दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक
उस समय के प्रसंग में कर्मों का विश्लेषण किया गया। अब प्रेम से राजा पुरञ्जन का आख्यान सुनो-
आसीत्पुरंजनो नाम राजा राजन्बृहच्छ्रवाः ।
तस्याविज्ञातनामाऽऽसीत्सखाविज्ञातचेष्टितः ।।
(श्रीमद् भागवत 4-25-10)
इसी पृथ्वी मंडल पर पुरञ्जन नाम का एक राजा था। उसके सखा का नाम अविज्ञात था। इसकी व्याख्या एवं सखा अविज्ञात के विषय में पीछे बतायेंगे। किसी दिन अपने प्रिय सखा अविज्ञात को छोड़कर राजा पृथ्वी मंडल में विचरण करने निकल गया। विचरण करते-करते वह जंगल में प्रवेश किया। वहाँ उसे एक बड़ी सुंदर नगरी, जिसके नौ दरवाजे थे मिली। वह राजा उसको सुरम्य देखकर उसके अंदर प्रवेश किया तो वहाँ उसे एक सुंदर रमणी बैठी हुई मिली। वह सुंदरी ग्यारह योद्धाओं से सुरक्षित थी और एक सर्प प्रहरी था जिसके पाँच सिर थे। सुंदरी के सौंदर्य से मोहित हो उस षोडशी से राजा पुरञ्जन पूछता है-
का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कस्यासीह कुतः सति ।
इमामुप पुरीं भीरु किं चिकीर्षसि शंस मे ।।
(श्रीमद् भागवत 4-25-26)
क एतेऽनुपथा ये त एकादश महाभटाः ।
एता वा ललनाः सुभ्रु कोऽयं तेऽहिः पुरः सरः ।।
(4 - 25 - 27)
राजा पुरञ्जन कहता है कि हे लोक सुंदरी ! तुम कौन हो? किस कुल की ललना हो और ये ग्यारह योद्धा कौन हैं? यह पाँच सिर वाला नाग कौन है? तो वह सुंदर बाला कहती है-
न विदाम वयं सम्यक्कर्तारं पुरषर्षभ ।
परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम् ।।
(4 - 25 - 33)
इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परम् ।
येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ।।
( 4 - 25 - 34)
एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद ।
सुप्तायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन्पुरीम् ।।
(4 - 25 - 35)
हे नर श्रेष्ठ ! यह तो मुझे विदित नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या गोत्र है, मैं किस कुल की हूँ? यह भी मैं नहीं जानती कि ये मेरे ग्यारह सखा कौन हैं।।। मैं जब इस नौ द्वारवाली पुरी में सो जाती हूँ तो यह पाँच फनवाला सर्प पुरी की रक्षा करता है।
प्रथम मिलन में ही दोनों एक-दूसरे पर आसक्त हो गए और राजा पुरञ्जन और वह सुंदरी दोनों प्रेमपाश में बंध गए। राजा मोहपाश में बंधकर गृहस्थ जीवन में पदार्पण किया। जब वह सुंदरी मोहित हो गई तो मोह का आदर समर्थन कैसे न हो-दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अंततोगत्वा कालांतर में दोनों के ग्यारह सौ पुत्र और एक सौ दस कन्यायें हुईं, समय बीतते गया। अब राजा और रानी दोनों का मृत्यु काल आ गया।
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तेमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।।
(गीता 8-6)
भगवान कृष्ण कहते हैं कि अन्तकाल में जो जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी भाव को वह प्राप्त होता है। मृत्यु काल में जिसका चिंतन करता है, प्राण के छूटने पर कोई भी हो, उसी भाव में स्थित हो जाता है। मृत्यु के समय में तो उसी भाव का चिंतन होगा जिस भाव में वह जीवन पर्यन्त आसक्त होगा। जीवन पर्यन्त जिस प्रिय वस्तु में उसकी आसक्ति होती है उसी का स्वरूप मरणकाल में होता है, वह उसी का स्मरण करेगा। यही तो आसक्ति का स्वरूप है। प्राप्ति में हर्ष हो और विछोह में दुःख हो। दोनों राजा पुरञ्जन और रानी पुरञ्जनी एक-दूसरे पर आसक्त थे। दोनों एक- दूसरे का चिंतन करते थे, तो मृत्यु के बाद राजा पुरञ्जन चूँकि रानी पुरञ्जनी का स्मरण करता था, उसी में वह आसक्त था इसलिए वह राजकुमारी वैदर्भी हुआ और रानी पुरञ्जनी मृत्यु के बाद मलयध्वज नामक राजकुमार हुई। मिशल उलट गई। यह अटल नियम है कि जाग्रत अवस्था में जिस विषय का चिंतन करता है स्वप्न में भी उसी का स्वप्न देखता है-उसी का स्वप्न होता है।
अब क्या-समय पाकर जब वे यौवनावस्था को प्राप्त हुए तो उनका फिर विवाह हो गया। राजकुमार मलयध्वज (जो पूर्वजन्म में रानी पुरञ्जनी थी) और विदर्भ राजकुमारी वैदर्भी (जो पूर्वजन्म का राजा पुरञ्जन था) दोनों प्रेम सूत्र में बंध गए। विवाह हो गया, राजा रानी पुनः बन गए और गृहस्थाश्रमोचित व्यवहार करने लगे। फिर समय पाकर वृद्धावस्था आई तो दोनों राजा मलयध्वज और रानी वैदर्भी वन में तप करने लगे। काल गति से राजा मलयध्वज की मृत्यु हो गई। (यह रानी पुञ्जनी थी पूर्वजन्म की) और राजा पुरञ्जन जो अभी वैदर्भी रानी है, मृतक के पास विलाप करने लगी।
इसी समय राजा पुरञ्जन का वह अविज्ञात सखा ब्राह्मण रूप से उपस्थित होकर उपदेश करता है। उसने आत्मतत्व का उपदेश किया। यह पुरञ्जनोपाख्यान् एक रूपक अलंकार है, समझो हमारे यहाँ ऋषि-मुनियों ने बड़े-बड़े महापुरुषों ने, जीव के कल्याण निमित्त सुंदर-सुंदर कथाओं के माध्यम से आत्मतत्व का निरूपण किया है। आत्मतत्व का बोध कराए हैं और जीव का आत्मकल्याण किये हैं। पुरञ्जन का अर्थ हुआ। 'स्व पुरं जनयति यः सः पुरञ्जनो जीवः।' अपने संकल्प से, वासना करके साढ़े तीन हाथ का जो शरीर है उसका स्वयमेव निर्माण करे, उसे कहते हैं पुरञ्जन (जीव), पुरञ्जन नाम जीव का है और जीव का सदैव सखा अविज्ञात है। सच्चिदानंद घनभूत परमात्मा, यह जीव का सखा है।
अविज्ञात-'न विज्ञातः इति अविज्ञातः ।' तो परमात्मा का विज्ञाता, उसका जानने वाला, उसका द्रष्टा, ज्ञाता सिवाय परमात्मा के और कौन होगा। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं-तो कैसे नहीं? सुनो-परमात्मा है सच्चिदानंद- सत्, चित, आनंद। तो आत्मा सत् स्वरूप है, चित (चेतन) है और आनंद स्वरूप है। बिल्कुल ठीक, परमात्मा से जीव को अलग करके मानो तो परमात्मा अलग और जीव अलग हो जायेगा और परमात्मा सत्य है तो जीव सत्य से भिन्न असत्य हो जायेगा। परमात्मा चित है। यदि वस्तुतः परमात्मा से जीव भिन्न है तो चेतन से भिन्न जीव जड़ होगा और परमात्मा आनंद स्वरूप है तो जीवात्मा से यदि परमात्मा को भिन्न मानते हो तो जीव दुःखरूप होगा। भिन्न मानते ही जीव असत्य, जड़ एवं दुःखरूप हो जाएगा। इसलिए ऐसे जीव को परमात्मा के जानने में क्या अधिकार है? यदि परमात्मा से अपने आप को जीव वस्तुतः भिन्न मानकर परमात्मा को जान लेता है तो फिर बन्ध्या का पुत्र शेर का शिकार कर सकता है। यह असंभव है। जीव अपने आप को परमात्मा से भिन्न मानकर यदि परमात्मा को जान लेता है तो आकाश में उड़ते हुए चिड़ियों के चरण चिन्ह वह देख सकता है। यह असंभव है। परमात्मा का नाम अविज्ञात है, उसको वही जान सकता है, जो स्वयं वही हो। उसका परिज्ञान दूसरे को नहीं हो सकता। अरे भाई ! समुद्र को नदी जानेगी कि समुद्र को समुद्र जानेगा? समुद्र को समुद्र ही जानेगा, नदी नहीं। देखो, सब हमको देखकर न कहो- समझो समुद्र को समुद्र जानेगा कि समुद्र को नदी जानेगी? अरे भाई ! देखो- दोनों समाज प्रेम से सुनो-जब नदी समुद्र को जानने के लिए चलती है तो यहाँ पर श्रुतियाँ कहती हैं-
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।।
(मुण्डप 3/2/8)
जब नदी समुद्र को जानने के लिये समुद्र के किनारे पहुँचती है तो नाम, रूप को परित्याग करके ही समुद्र को जानती है। समुद्र को जानकर नदियाँ समुद्र हो जाती हैं। फिर वहाँ पर गंगा, यमुना आदि नदियाँ ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलती, नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। प्रवाह नदी का रूप है। जब वह समुद्र से मिली तो सब कुछ अपनापन छोड़ दिया-नाम, रूप के त्याग के बाद फिर शेष क्या रहा? नदी भी समुद्र हो गई। नदी यदि समुद्र में मिलने पर अपना अस्तित्व (वजूद) रखती है तो जान लो अभी समुद्र से दूर है और इसलिये जब वह समुद्र से मिली तो फिर नदी नहीं रह गई, स्वयं ही समुद्र हो गई। अच्छा, अब देखो-समुद्र नाम समुद्र को किसने दिया? नदी ने ही समुद्र नाम दिया-नहीं तो समुद्र कहाँ? समुद्र कहेगा कौन? तो फिर नदी नहीं रही, न समुद्र। अच्छा समुद्र हो जाने पर नाम, रूप का त्याग करने पर फिर उसका अस्तित्व नहीं रहा। तो फिर नदी की अपेक्षा से समुद्र था। तो समुद्र कहेगा किसको? समुद्र में मिलने के बाद जब नदी हो तब तो समुद्र कहा जाए। आज के पहिले जब गंगा नाम, रूप छोड़कर समुद्र हो गई (यह बारीक चीज है, जरा ध्यान से समझना) तो न पहिले की याद, न अब की। समुद्र का परिज्ञाता हो तब तो समुद्र कहे। इसी प्रकार जीव, भगवान को प्राप्त करके जीवभाव (नाम, रूप) त्याग कर पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है। 'स्व' का जब बोध हो गया। बद्ध था, अब मुक्त हो गया, अज्ञानी था, ज्ञानी हुआ इत्यादि। अतीत और वर्तमान की स्मृति नहीं रहती। यदि यह याद है तो यारों! जान लो वह अभी भगवान से सैकड़ों मील दूर है। खचेडू का खचेडू ही रहा।
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।।
इसलिये मानसकार कहते हैं-
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ।।
श्रीराम को जानकर राम ही हो जाता है।
ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति ।।
(मुण्डक 3/2/9)
परमात्मा को जानकर परमात्मा ही हो जाता है। याद रखो, परमात्मा को जानने का जीव की अनधिकार चेष्टा है। परमात्मा से भिन्न जीव को परमात्मा को जानने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए परमात्मा अविज्ञात है। हाँ जी-
ग्यारह योद्धा कौन हैं? बुद्धि रूपी पुरञ्जनी के पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय एवं ग्यारहवाँ मन, यही वे ग्यारह योद्धा हैं। पाँच फण वाला सर्प प्राण हैं (प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान), पाँच सिर वाला (प्राण वायु) बुद्धि रूपी पुरञ्जनी जब सो जाती है तो नव द्वार वाली नगरी (शरीर) की रक्षा करता है। एक-एक इन्द्रियों के एक-एक सौ विकार बुद्धि में होते हैं, यही ग्यारह सौ पुत्र हैं और बुद्धि की एक सौ दस प्रकार की जो वृत्तियाँ, यही एक सौ दस कन्यायें हैं। इस कथा का यही सारांश है। जीव रूपी पुरञ्जन का परम सखा परमात्मा सच्चिदानंद घनभूत भगवान ही है। यही अविज्ञात सखा पुरञ्जन जीव को उपदेश करता है।
आनन्द कन्द श्री सच्चिदानंद घनभूत परमात्मा ब्राह्मण का रूप लेकर उपदेश करता है-
का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि ।
जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ ह ।।
(4/28/52)
का त्वम्, कस्य असि, अयम् कः-तू कौन है? ये कौन है? ओहो-तू विलाप किसके लिए कर रही है। तू स्वयं अपने आप को देख, समझ और इस अज्ञान को छोड़-इतना अज्ञान, इतनी महान भूल। तुमने अपने आप को साढ़े तीन हाथ का देह माना, स्त्री माना-
अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः ।
न नौ पशयन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि ।।
(4/28/62)
मैं जो हूँ, वही तू है। अन्यः न-दूसरा नहीं। त्वमेवाहं-तू ही मैं हूँ और मैं ही तू है। मुझ परमात्मा और तुझ जीवात्मा में कवि महात्मा जन कभी छिद्रमात्र का भी अंतर नहीं देखते। अच्छी तरह समझ लिया तो आत्मभाव को प्राप्त हो जाएगा और यदि भेद माना तो जीवभाव में पड़ा रहेगा। इतना ही भेद है-
यथा पुरुष आत्मानमेकमादर्शचक्षुषोः ।
द्विधाभूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः ।।
(4/28/63)
जिस तरह कोई पुरुष हाथ में दर्पण लेकर अपना मुँह देखता है तो शीशे के भीतर उसका ही प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। इसे वेदांत में आभासवाद कहते हैं। जिस प्रकार बिम्ब और प्रतिबिम्ब का भेद है, इसी प्रकार मुझ परमात्मा और जीव का भेद है। बिम्ब और प्रतिबिम्ब का यह भेद पूर्णतया सोपाधिक है, निरुपाधिक नहीं।
प्रतिबिम्ब-सखे ! किस तरह? तू और है और मैं और हूँ।
बिम्ब कहता है-प्यारे प्रतिबिम्ब देख तू मुझसे अलग नहीं है। मैं ही तू है और तू ही मैं हूँ। सामने से शीशा हटा लेने पर यदि तू दिखाई दे तब तू भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। मेरा और तेरा भेद शीशाकृत भेद है। यह सोपाधिक भेद है, निरुपाधिक भेद नहीं। देखो, समझो अब दो हो गए न, बिम्ब और प्रतिबिम्ब, हटा लो शीशे को-तो प्रतिबिम्ब न रहा और समझो तो बिम्ब भी न रहा। यदि प्रतिबिम्ब नहीं तो बिम्ब भी न रहा। अरे यार ! जब पुत्र होगा तभी तो पिता होगा, पुत्र बिना पिता कैसे? उसको पिता कौन कहेगा? पुत्र नहीं तो पिता कहाँ? बेटा से बाप या बाप से बेटा? सब हमारे तरफ हो गए। मौज में मौज मिला रहे हैं। भैया ! पुत्र होगा तब तो पिता कहने वाला होगा, तो पुत्र के भाव में पिता का भाव है और पुत्र के अभाव में पिता का अभाव है। अब जो शेष रह गया वह न पिता है, न पुत्र है। देखो यह बालक बैठा है आपके सामने, अभी तक इसका नाम पिता नहीं है। हाँ, इसी में पिता और पुत्र का भाव निहित है, क्योंकि आगे यही तो पिता होगा। पिता, पुत्र दोनों नामका आश्रय यह बालक है। यदि पुत्र न रहा, तो पिता भी न रहा। अब रह गया सिर्फ भास, जो बिम्ब और प्रतिबिम्ब दोनों का आधार है। इसी तरह जाग्रत और स्वप्न जिस समय मुझ आत्मा के समक्ष, मन रूपी शीशा आ गया, बस, जीव रूप प्रतिबिम्ब भासने लगा-इस तरह समझो कि जीव रूपी प्रतिबिम्ब और ईश्वर रूपी बिम्ब दोनों पैदा हो जाते हैं। जाग्रत अवस्था में मुझ आत्मा का जो प्रतिबिम्ब उसे जीव कहते हैं और जीव प्रतिबिम्ब की अपेक्षा से मुझ आत्मा का ही नाम बिम्ब ईश्वर हो जाता है। इसी तरह स्वप्नावस्था में भी आत्मा में मन रूपी शीशे उपाधि के कारण जीव और ईश्वर ये दोनों विकल्प भासते हैं। परन्तु, सुषुप्ति अवस्था में मन रूपी शीशा नहीं रहता, मन अज्ञान में लीन रहता है तो दोनों की कल्पना नहीं होती। दोनों विकल्पों का सुषुप्ति अवस्था में अभाव हो जाता है, परन्तु 'मैं' आत्मा रहता हूँ। उस अवस्था में यदि 'मैं' आत्मा न रहूँ तो सुषुप्ति के आनंद का अनुभव कौन करेगा? इस तरह से जिस आधार पर ईश्वर और जीव की कल्पना होती है, वह आधार मन सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहता। जो जाग्रत में वही 'मैं' स्वप्न में और जो 'मैं' जाग्रत और स्वप्न में वही 'मैं' सुषुप्ति गाढ़ी नींद में। जीव और ईश्वर दोनों का अधिष्ठान 'मैं' ही हुआ बिल्कुल स्पष्ट है। जी हाँ-
निरुपम नित्य निरंशकेऽप्यखण्डे मयिचिति सर्व विकल्पादि शून्ये ।
घटयति जगदीश जीव भेदं त्वघटित घटना पटीयसी माया ।11।।
विद्वजनों ! सुनो-मैं आत्मा नित्य सच्चिदानंद निरुपम (उपमारहित) हूँ। 'मैं' आत्मा की मिशाल नहीं। समस्त विकल्पों से रहित, परन्तु वाह री माया, जो मुझ निरुपम, नित्य, निरंश आत्मा में जीव और ईश्वर दो की कल्पना कर लेती है। जो चीज न घटने वाली वह घटा कर बता देती है।
निरुपम नित्य निरंशकेऽप्यखण्डे मयिचिति सर्व विकल्पादि शून्ये ।
घटयति जगदीश जीव भेदं त्वघटित घटना पटीयसी माया ।।1।।
जो सुनने में आये उसे प्रत्यक्ष करके दिखा देना माया का ही काम है।
श्रुति शत निगमान्त शोधकानप्यहह धनादि निदर्शनेन सद्यः ।
कलुषयति चतुष्पदाद्यभिन्नान् त्वघटित घटना पटीयसी माया ।।2।।
श्रुतिशत निगमान्त शोधकाप्यहह धनादि निदर्शनेन सद्यः अहह ! बड़े ही दुःख एवं आश्चर्य का विषय है कि बड़े-बड़े प्रज्ञावान विद्वान जो वेदों एवं वेदों के 'तत्वमसि' इत्यादि महावाक्यों का संशोधन करते हैं, वे भी धन के लोभ में ऐसे फँसते हैं कि कलुषयति चतुष्पदाद्यभिन्न त्वघटित घटना पटीयसी माया- चार पैर के पशु में और ऐसे विद्वान में कोई भेद नहीं रहता। विद्वानों पर ठगनी माया हुँमक-हुँमक कर चलती है, उन्हें बरबाद कर देती है। निगमों की व्याख्या करेंगे-कहेंगे कि संसार असार है। प्रदर्शन तो ऐसा करेंगे कि संसार मिथ्या है, नाशवान है, बन्ध्यापुत्र है, रज्जौसर्पवत् है और आसक्ति है वित्त में। कलंकित पदार्थों में मन पिरोये रहते हैं, दूषित पदार्थों में पड़ते हैं। वाह री माया, अघटित को घटित करके बता देती है। ऐसी माया ठगनी है कि विद्वानों के और चार पैर के पशु में कोई अंतर नहीं रखती। पशुवत् वृत्ति उनकी हो जाती है। अघटित घटना पटीयसी माया-न घटने वाली बात को घटा कर बता देती है माया।
सुखचिदखण्ड विबोधमद्वितीयं वियनलादि विनिर्मिते नियोज्य ।
भ्रमयति भवसागरे नितान्तं त्वघटित घटना पटीयसी माया ।।३।।
मुझ अव्यक्त ब्रह्म में विकृत संसार की भावना कर देती है। पंच महाभूतों की कल्पना कर देती है। पंच महाभूत ही नहीं वरन तन्मात्रायें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर, चतुष्टय अन्तःकरण मन, बुद्धि, コ चित्त, अहंकार, पंच प्राण-प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय आदि की कल्पना कर देती हैं। यद्यपि ये मुझमें किसी काल में भी नहीं हैं, तब भी वाह री ठगनी माया ! इनकी कल्पना तू मुझ आत्मा पर कर देती है। ये मुझमें वस्तुतः नहीं है, परन्तु कालादि की भावना माया पैदा कर देती है। मुझ आत्मा में नानात्व आदि का विकल्प कर देती है। जिसके चक्कर में पड़कर जीव अनादिकाल से भ्रमित है।
अपगत गुण वर्ण जाति भेदे सुख चित विप्र विडाद्यहंकृतिंच ।
स्फुटयति सुत दार गेह मोहं त्वघटित घटना पटीयसी माया ।।4।।
मुझ आत्मा में वर्ण और आश्रम आदि का भेद पैदा कर देती है कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूँ-मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यासी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ आदि। आत्मा सर्व उपाधियों से रहित है, परन्तु यह सब होते हुए भी यह माया मुझ विशुद्ध निरञ्जन, अवांगमनसगोचर आत्मा में वर्णाश्रम आदि का मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यासी हूँ आदि की कल्पना कर देती है। ढूँढो तो उसका कहीं भी पता नहीं चलेगा।
विधि हरिहर भेदमप्य खंडेवतविरचरय बुधानपि प्रकामम् ।
भ्रमयति हरिहर विभेद भावान् त्वघटित घटना पटयसी माया ।।6।।
आश्चर्य है कि बड़े-बड़े विद्वानों के भी हृदय में एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्म में जो माया हरि, हर दो का भेद कर देती है। इसलिए जो बात नहीं घटने वाली वह भी घटा कर बता देती है।
जिस समय भगवान श्रीराम समुद्र तट पर रामेश्वर विजय लिंग की स्थापना लंका जाने के पेश्तर किए तो श्रीराम ने विजय लिंग का नामकरण किया-श्री रामेश्वर। अब वहाँ पर इस नाम के भाव में चख-चख पैदा हो गया कि वास्तव में श्री रामेश्वर का क्या भाव हो? इसका क्या अर्थ हो, इस विषय में चर्चा हुई।
रामस्तत्पुरुषं वेत्ति बहुब्रीहं च शंकरः ।
रामेश्वरः पदे प्राप्ते कपयः कर्मधारयः ।
यो हरिः सः शिवः साक्षात् यः शिवः सः स्वयं हरिः ।
द्वयोर्भेदं यो जानाति स याति नरकं प्रति ।।
रामस्य ईश्वरः-रामेश्वरः षष्ठी तत्पुरुष समास। श्रीराम के जो ईश्वर है रामेश्वर। इसलिए श्रीराम ने यही अर्थ किया कि जो राम के ईश्वर हैं इसलिय रामेश्वर। तो श्री शंकर भगवान ने यह अर्थ नहीं माना। रामः ईश्वरो यस्य सः रामेश्वरः-बहुब्रीहि समास-श्रीराम है ईश्वर जिसके वह रामेश्वर। तब कि किसको स्वामी कहें और किसको सेवक। वानरी सेना नल, नील, जामवन्न हनुमान, सुग्रीव, अंगद इत्यादि ने कर्मधारय समास माना। इसी अर्थ को स्वीका किया रामश्चासौ ईश्वरः, रामेश्वरः- राम ही जो ईश्वर और ईश्वर ही जो राम अर्थात् जो राम है, वही शिव है और जो शिव है, वही राम है। तो श्री हरिहा में जो भेद मानता है उसके लिए ठगनी माया ही कारण है। यह सब ठगनी माया का ही खेल है। सत्य नहीं है। तो फिर देखो-कभी-कभी लोग हमसे पूछ बैठने हैं कि स्वामी जी ! श्री शंकर जी की उपासना कैसे और श्री विष्णु की कैसे करें? अरे ! जब इनमें भेद ही नहीं तो उपासना में क्या भेद है। इसलिए कोई हमसे पूछता है तो हम यह सलाह देते हैं कि यदि तुम शंकर के उपासक हो तो श्री शंकर जी का अभिषेक इस मंत्र से करो-
शान्ताकारं भुजगनशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम ।
लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं ।
वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ।।
इस मंत्र से श्री भगवान शंकर का अभिषेक स्नान कराएँ और खूब डटकर तुलसी पत्र चढ़ायें और जब भी श्री विष्णु की आराधना करें तो इस मंत्र से करें।
ॐनमो शम्भवाय च मयोभवनाय च नमः शंकराय च
महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ।
(यजुर्वेद 16-41)
और खूब बेल पत्र चढ़ायें। जब तक तुम्हारी यह दृष्टि नहीं होती, तुम्हारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यासी आदि वर्णाश्रम का अभिमान रहेगा, तब तक भगवान की प्राप्ति होना दूर है। अरे! भगवान में भी भेद। इन भेदवादियों ने भगवान को भी अछूता नहीं छोड़ा। वर्ण, वर्ण में भेद, आश्रम, आश्रम में भेद, जाति, जाति में भेद। ठीक है भैया-मौज करो। हाँ और चलो थोड़ा बतायें। श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड में चलें-
परवस जीव स्ववस भगवन्ता। जीव अनेक एक श्रीकंता ।।
तो इसका अर्थ क्या होगा? अरे ! वही, जो तुम करोगे। परबस जीव-वैसे तो अमूमन अर्थ है कि जीव जो है वह परवश है और भगवान स्ववश है, जीव अनेक हैं और भगवान एक है। यदि ऐसा अर्थ लगायें तो बिगड़ जायेगा? जब तक परवश है तब तक वह जीव है और इसमें जिसको शंका हो हमारे पास आयें। अपने आप 'मैं' आत्मा को जब जीव मानता है तब परवश है और अपने आप 'मैं' आत्मा को जब भगवान जानता है तब स्ववश है। जो अपने आप को स्ववश जानता है वह ईश्वर है ही, मानने का सवाल ही नहीं। ध्यान रखो-यहाँ पर जानना कहा गया है। परवश मानना ही तो जीवभाव है और अपने आपको जो स्ववश जाना वही भगवान। बस, यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब इसकी अपील ही नहीं हो सकती। यहाँ पर जीव और ईश्वर का भेद बताते हैं और फिर रामायणकार आपको आगाह करते हैं कि भैया! इस भेद को असली रूप में न समझ बैठना, यह मुधा भेद है।
मुधा भेद यद्यपि कृत माया। बिनु हरि जाय न कोटि उपाया ।।
यहाँ पर जो भेद बताया गया है, जीवात्मा और परमात्मा में यह मिथ्या है, मायाकृत है, सत्य भेद नहीं है। अरे! यह भेद मुधा है, सोपाधिक है, निरुपाधिक नहीं। मतलब, देखो, सामने पेण्डाल के दोनों तरफ दीवाल है तो एक दीवाल से दूसरे दीवाल तक एक ही स्थान है, परन्तु जब एक रस्सी इनके बीच में बांध दी जाती है तो फिर इस पार और उस पार की कल्पना स्वयं हो जाती है। इस पार और उस पार दो नाम हो जाएगा और जब रस्सी निकाल दो तो न इस पार और न उस पार। भेद का पता ही नहीं रहेगा। स्वयंपाकी लोग जो होते हैं जानते हो- चूल्हे के पास एक लकीर खींच देते हैं। तब इस पार चौका हो जाता है। अब देखना, भला कोई लकीर के भीतर आ जाए। कोई कुछ चीज देने आएगा तो बिगड़कर कहेंगे, उधर, उधर ही रहो ओ हो ! जमीन एक ही है, परन्तु वाह रे मनीराम, कहते हैं वहीं पर रख दो- भैया ! उधर ही रखना। जबकि उस जमीन पर स्वयं पाकीजी बैठे हैं और उसी जमीन पर वह चीज है और चीज लाने वाला भी उसी एक ही जमीन पर खड़ा है। तो रेखा से ही तो भेद पड़ा इस पार और उस पार का, परन्तु सब पढ़कर भी पृथ्वी का ज्ञान नहीं हुआ। जमीन का ज्ञान नहीं है, तभी यह भेद है। इस पार और उस पार की कल्पना होती है जबकि जमीन जगह एक ही है। तो जीव भाव और ब्रह्मभाव, जीव और ईश्वा इनका आधार 'मैं' आत्मा ही हूँ।
एकात्मके परे तत्वे भेदवार्ता कथं भवेत् ।
सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः ।।
यदि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है तो सुषुप्ति अवस्था (गाढ़ी-नींद) में जीव और ईश्वर का भेद विद्यमान होना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता। सुबह उठने से ही भेद की प्रतीति होती है। तो फिर सुषुप्ति में जीव और ईश्वर का भेद कहाँ चला जाता है?
नुक्ते के हेरफेर से खुद से जुदा हुआ ।
नुक्ता जो देखा गौर से तो खुद ही खुदा हुआ ।।
उर्दू भाषा में जीम से लिखा जाता है जुदा और उस नुक्ते को उठाकर उसके सिर पर रख दो तो वह हो जाता है खे-खुदा बन जाता है। अरे यार! सिर्फ बिन्दी ही तो हटाना है-क्या कुछ करना है?
नुक्ते के हेरफेर से खुद से जुदा हुआ ।
नुक्ता जो देखा गौर से तो खुद ही खुदा हुआ ।।
जी हाँ, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह कहा करते थे कि एक नुक्ता ने किया खुदा से मुझको जुदा। खुदा को कहते हैं वाहिद। वाजिद में जो नुक्ता है उसे हटा दो तो वह शब्द वाहिद बन जाता है।
आत्मजिज्ञासुओं ! अरे, इस पर कभी गौर किया है? चलो अब दृष्टांत द्वारा बताएँ। पंचदशीकार स्वामी विद्यारण्य जी दसवें पुरुष का दृष्टांत देते हैं। किसी स्थान से दस आदमी अपने देश को लौट रहे थे। उनका स्थान नदी के उस पार था। नदी बड़ी थी। नदी पार होकर उन्हें जाना था। जब नदी के पास दसों पहुँचे तो वहाँ पर नदी के पार जाने के लिये नाव, डोंगा, किश्ती कुछ नहीं था। नदी का पाट चौड़ा था। नदी गहरी थी, पानी भी ज्यादा था। क्या करें, नदी में सभी कूद पड़े और तैरते हुए सभी सही सलामत पार आ गए। दसों तैरकर उस पार नदी के किनारे खड़े हो गए। उन दसों में एक लालबुझक्कड़ था। जिसको अक्ल की बदहजमी थी। किसी-किसी को अक्ल की बदहजमी रहती है। तो वह यह सोचने लगा कि चलो पहिले ठीक तरह से देख लें कि हम दसों पार हो गए या कोई बह तो नहीं गया। लगा गिनती करने, एक-एक करके सिर पर हाथ रखकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक गिन गया और अपने को गिनना भूल गया। तो नौ ही रहे। इसी तरह दो-चार बार गिनती करने पर भी नौ ही शेष रहते थे तो वह दसवें का पता नहीं लगा पाया। नौ तक ही गिन पाता था। दूसरे साथियों ने पूछा कि क्या बार-बार गिन रहे हो क्या तुम्हें कोई शंका है? वह अक्ल की बदहजमी वाला घुड़ककर कहता है-क्या शंका? अरे ! देखते क्या हो दसवें का तो पता ही नहीं है-शायद दसवाँ डूब गया। क्या दसवाँ डूब गया। अब सब परेशान, दूसरा उठकर गिनने लगा। वह भी सब के सिर पर हाथ रखकर 1, 2, 3, नौ तक गिना और अपने को भूल गया। दसवाँ गायब, उसने भी दसवें को नहीं पाया। फिर क्या-सभी नौ आदमी एक-दूसरे के सिर पर हाथ रख गिने और नौ तक ही गिनते रहे। कारण सभी अपने को गिनने में भूल करते रहे। तो सचमुच में दसवाँ डूब गया। अब यह सभी को निश्चय हो गया कि दसवाँ सचमुच में डूब गया। यद्यपि दसों वहाँ हैं, परन्तु इस तरह अलग-अलग भूलते जाते अर्थात् दसों ही बह गए। यद्यपि सभी मूसरचंद वही हैं। फिर क्या, कोलाहल मच गया हाय रे दसवाँ, हाय रे दसवाँ, कभी पत्ते की आड़ में कभी नदी में खोजें, कहीं दसवाँ नदी में अटका हो तो मिले। खोजने वालों को उनका दसवाँ न मिला, क्योंकि खोजने वालों से अगर दसवाँ भिन्न हो तो मिले। कुछ गुमा हो तो मिले। वे लोग छाती पीट-पीटकर रोने लगे। हाय रे मेरा दसवाँ कह करके। हाँ भाई, कोई किराये से रोने वाला मिले तब तो, वे ही लोग रोने लगे। उसी समय उधर के एक बूढ़ा, मुसाफिर निकला। इस तरह से उन लोगों को रोते-पीटते देख, वह पूछने लगा-भाइयों! क्यों रोते हो? क्या बात है? तो वे कहने लगे कि हम लोग दस थे, दसों नदी पार किये, परन्तु हम नौ ही बाहर आये, हमारा दसवाँ नहीं निकला, संभव है वह नदी में बह गया। हम लोग अपने दसवें के लिए रो रहे हैं। बूढ़ा मुसाफिर अक्लमंद था। वह मन में धीरे से सभी को गिन लिया और देखता है कि दस के दस मूसरचंद सभी मौजूद हैं। बेवकूफी के कारण दसवाँ-दसवाँ चिल्ला रहे हैं। वह मन ही मन गिनती लगा लिया और कहता है कि भाई! एक बार मैं भी गिनती लगाऊँ तब मालूम हो। तो वे कहते हैं कि हम अभी तक गिनती ही तो लगाए हैं तो बूढ़ा मुसाफिर कहता है कि ठीक है, तुम लोग मेरे सामने गिनती लगाओ। बूढ़े के कहने से वे गिनती जैसे पहिले लगाये थे 1, 2, 3, 4....9 की गिनती लगाए और फिर अपने को भूलकर दसवें के लिए हाथ मसलने लगे। इस तरह दसों ने गिनती लगाई और हर एक अपने को गिनना भूलते रहे। बूढ़ा समझ गया कि सभी की बुद्धि खराब है। सभी का दिमाग फेल है। तो वह कहता है कि तुम लोगों का दसवाँ तुम्हीं लोगों में है। तो वे कहने लगे कि फिर वह मिलता क्यों नहीं? अज्ञानियों की विकट खोपड़ी होती है। वह बुड्ढा कहता है कि देखो-क्या तुम दसवाँ देखना चाहते हो? मेरे पास आओ। एक-एक का कान पकड़कर, हाथ पकड़कर हाँ भाई! हाथ पकड़ना चाहिए, अरे! जो रिसीव्ह करता है हाथ मिलाता है न। देखो-एक मिनट में मैं दसवें का पता लगाता हूँ। फिर सबके सिर में हाथ रखकर 1, 2, 3... करते-करते दसवें के गाल पर तमाचा लगाया कि जिस दसवें को ढूँढ़ रहा है वह दसवाँ तू। मिला तुम्हारा दसवाँ? इसी तरह सबको पकड़-पकड़कर दसवाँ दिखा दिया। दसों को तमाचे पड़े। जब तक दसवाँ नहीं मिला था तब तक दसवें के लिए रो रहे थे और दसवाँ वे ही सब थे। दसवाँ जितना दूर था उतना ही नजदीक, इसकी भी कोई सीमा नहीं।
अनादिकाल से नाना प्रकार के साधनों से दुनियाँ भटक रही है। किसी की बात मानता नहीं। किसी की शिक्षा मानने को तैयार नहीं, परेशान है। जब कोई संत महात्मा महान पुरुष 'तत्वमसि' महावाक्य द्वारा (जैसा ऊपर दसवाँ दिखाया गया) स्वयं में स्वयं को परमात्मा लखा देते हैं। सभी परमात्मा को ढूँढ रहे हैं। परन्तु कभी भी विचार किया कि मैं कौन हूँ? कभी भी सोचा-विचारा कि लगे परमात्मा को ढूँढने के लिये। परमात्मा के पीछे डंडा लिए घूम रहे हैं। पहिले समझो कि मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या हूँ। कभी भी अपने को समझने की कोशिश नहीं की। अब इसी की शान में एक गजल सुनाता हूँ-
हूँ जज्बे जलवागर सबमें इकसां, दीवाना होकर जो हमने देखा ।
जज्बे-ठसाठस, जलवागकर-प्रकाशक
गई जहन्नुम में सारी दुनियाँ बेताब होकर जो हमने देखा ।।1।।
वाह जी वाह-जहन्नुम में-गर्त में-भाड़ में।
मैं हूँ सभी का हूँ सबसे आला, तकरीर मेरी न इस जहाँ में ।
बताने वाले खामोश बैठे, नाचीज होकर जो हमने देखा ।।2।।
आत्मा होने के नाते 'मैं' किसका नहीं हूँ, किसमें नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, कहाँ नहीं हूँ-अरे ! लकड़ी, तख्त, खिड़की, किवाड़, कुर्सी, मेज, बेंच इत्यादि किसमें नहीं है, किसकी नहीं है, क्या नहीं। बिल्कुल इसी तरह आत्मा व्याप्त है।
मैं हूँ सभी का हूँ सबसे आला, तकरीर मेरी न इस जहाँ में ।
बताने वाला खामोश बैठे, नाचीज होकर जो हमने देखा ।।2।।
तकरीर-व्याख्यान
'मैं' आत्मा की कोई व्याख्या नहीं, 'मैं' पर कोई व्याख्या नहीं होता। शास्त्र, वेद, पुराण, सब भगवान आत्मा की महिमा गाते हैं। जो आत्मा शास्त्र, वाणी, मन, बुद्धि से परे हैं-तो फिर क्या वाणी 'मैं' आत्मा की व्याख्या करने में समर्थ है। 'मैं' वाणी का विषय नहीं हूँ। मन, बुद्धि का विषय नहीं हूँ। भगवान आत्मा व्यापक है, अमर है, परिपूर्ण है, उसकी व्याख्या वाणी क्या कर सकती है। शास्त्र, वेद, पुराण सब श्री भगवान आत्मा की महिमा की ही व्याख्या कर सकते हैं। जब वे स्वयं परिच्छिन्न है तो वे मुझ आत्मा की क्या व्याख्या कर सकते हैं।
मैं हूँ सभी का हूँ सबसे आला, तकरीर मेरी न इस जहाँ में ।
बताने वाले खामोश बैठे, नाचीज होकर जो हमने देखा ।।2।।
जगत में देखते ही हैं। शिष्टाचार से जब कोई किसी के पास जाता है तो उसको पूछता है-कहिये, आपका दौलतखाना कहाँ है? तो वह कहता है-मेरा गरीबखाना लखनऊ में है, इलाहाबाद में है। हुजूर के मुकाबिले में नाचीज हूँ। तो नाचीज किसको कहते हैं? अपने आपको कुछ भी माना, तब तक वह चीज है। तब तक मैं चीज हूँ जब तक मैं अपने आपको कुछ भी मानता हूँ। जब अपने आपको कुछ नहीं मानता, अपने आप 'मैं' को 'मैं' ही जानता हूँ तब वह नाचीज हो गया। मानापमान से परे हो गया। तो तू भी नाचीज हो जा। 'मैं' आत्मा की कौन व्याख्या करेगा-आत्मा की व्याख्या नहीं हो सकती। जब कुछ कहा नहीं जा सकता तो आत्मज्ञानी संत महात्मा क्या कहें, आत्मा के लिए सब खामोश बैठे हैं। इसका रियलाइजेशन (दर्शन) कब हो? जब वह कुछ भी मानना मिटा चुका-नाचीज होकर हमने देखा-बताने वाले खामोश बैठे हैं।
मैं हूँ सभी का हूँ सबसे आला, तकरीर मेरी न इस जहाँ में ।
बताने वाले खामोश बैठे, नाचीज होकर जो हमने देखा ।।2।।
हूँ जज्बे जलवा... वाह जी वाह-
जो कुछ भी माना खुद को ही माना मैंने ही माना ये भूल-भूलैया ।।
यह खेल कैसा पर्दानशीं का परदा उठाकर जो हमने देखा ।13।।
और है कौन सिवाय मुझ आत्मा के- यह खेल कैसा पर्दानशीं का परदा उठाकर जो हमने देखा-वाह जी वाह- परदा के अंदर रहने वाला-क्या खूब, परदा उठाकर जो हमने देखा-विकल्प, मान्यता यह सब माया का परदा है। 'मैं' आत्मा इसके अंदर रहने वाला परदानशीं हूँ-भाई ! परदा उठाना पड़ेगा। आत्मा का दर्शन करना है तो मान्यता जगत से ऊपर उठो। विकल्प छोड़ दो-परदा फाड़दो-मान्यता परदा हैं तो उसे उठाकर फेंक दो-विकल्पों को छोड़कर परदानशीं का दर्शन हो सकता है। परदा उठाने से ही मालूम पड़ा। विकल्प का नाश हुआ-
हूँ जज्बे जलवागर सबमें इकसाँ, दीवाना होकर जो हमने देखा ।
अरे !
भटकती दुनियाँ दहरोहरम में दिले दफीना हुआ न हासिल ।
अनादिकाल से जंगल, पहाड़, नदी, गुफा सब जगह ढूँढ रहे हैं। मुद्दत बीत गई, दिन पर दिन निकल गया भटकते-भटकते-हाँ भाई सभी भटक रहे हैं, परन्तु दिल के अंदर ही जो खजाना गड़ा है-दिल दफीना मन के अंदर गड़ा हुआ खजाना ('मैं' आत्मा) न मिला। अनादिकाल से दुनियां परेशान है- भटकती है।
भटकती दुनियाँ दहरोहरम में दिले दफीना हुआ न हासिल ।
दिले दफीना तलाशगर खुद, नजर उठाकर जो हमने देखा ।।4।।
समझना जरा-दिले दफीना- 'मैं' आत्मा को तलाश करने वाला स्वयं (खुद) ही है दिले दफीना है। कैसे मिले? दुनियाँ भटक रही है, खोज रही हैं- हूँ जज्बे जलवागर सबमें इकसाँ, दीवाना होकर जो हमने देखा । गई जहन्नुम में सारी दुनियां, बेताब होकर जो हमने देखा ।।
और क्या-
मेरी हुकूमत से शम्स रोशन, कमर सितारे हैं जगमगाते ।
मुझ आत्मा की हुकूमत (आज्ञा सूत्र) में सूर्य, चन्द्र, सितारे आकाश में नाच रहे हैं। इन सबका शासक कौन है?
य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः
शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।।
(वृहदा 3/7/9)
जो आदित्य (सूर्य) के अंदर व्याप्त है। जिसको आदित्य नहीं जानता, जो आदित्य को जानता है, आदित्य ही जिसका शरीर है, आदित्य पर जो शासन करता है, जो आदित्य का नियमन करता है, वह अविनाशी अन्तर्यामी अमृत आत्मा तू है।
क्या मजाल है कि सूर्य, चन्द्र की गति में एक मिनट भर का भी फर्क हो जाए, घड़ी लेट हो जाए, परन्तु सूर्य की घड़ी लेट नहीं होती। जिस दिन जिस समय उसे उदय होना है, बिल्कुल ठीक टाइम पर वह उदय होता है। उसी नियम से कार्य होगा-बिल्कुल इधर-उधर नहीं, कभी सोचा कि किसकी आज्ञा से सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारागण कार्य कर रहे हैं? किसका शासन है?
मेरी हुकूमत से शम्स रोशन, कमर सितारे हैं, जगमगाते ।
सच में मुबारक बेमुल्कशाही, कुर्बान होकर जो हमने देखा ।।5।।
तो भैया ! कुरबानी है यहाँ बिना सिर के हो जाना, यही करना चाहिए। अभी, यहीं अनुभव करो, जितने यहाँ बैठे हो-जब तक तुम आत्म तत्व 'मैं' को नहीं समझे हो-जब तक तुम अपने से अलग मानते हो, तभी तक कुदरत तुम्हारा नियमन करती है, तुम्हारे ऊपर शासन करती है। प्रकृति तुम्हारा शासक है। हाँ-प्यारे ! मान्यता जगत से परे होकर आओ। अपने 'मैं' को जानो तब फिर 'मैं' ही शुद्ध तत्व रह जाएगा। रह गया शुद्ध तत्व भगवान आत्मा-बन्दर को जैसे बाजीगर नचाता है उसी प्रकार आत्म तत्व को बिना जाने प्रकृति तुम्हें नचाती है। उसके ऊपर शासन करती है। मान्यता जगत के बाहर जिस दिन प्रकाश में आ जाओगे तो तुम्हीं शासक हो, फिर क्या कमी है। तुम हो जाओगे शासक ! मुबारक है-मुबारक है-धन्यवाद। अरे! जिसके पास एक अंगूठा रखने भर की भी जमीन कहने के लिए नहीं है, अंगूठा टेकने की जगह नहीं है, वह बिना ताज के बादशाह बना है।
सच में मुबारक बेमुल्कशाही, कुर्बान होकर जो हमने देखा ।।5।।
हूँ जज्बे जलवागर सबमें इकसाँ, दीवाना होकर जो हमने देखा ।
हमेशा लहराता 'मुक्त' दरिया, हुआ है. गर. काब ए सारा आलम ।
पता नहीं मैं था कौन क्या हूँ, मस्ताना होकर, जो हमने देखा ।। 6 ।।
कब देखा? मस्ताना होकर-जब हमने देखा।
मस्ताना डोलत फिरै, ज्यों सरकारी साँड़ ।
डर काहू की है नहीं, खसम बिना जस राँड़ ।।1।
गाँवों में देखे होंगे, एक सरकारी और एक लोकल दो प्रकार के साँड़ होते हैं। लोकल साँड़ को कभी-कभी लोग हल में जोत लेते हैं, कांजी हौस में भी दे देते हैं और भैया ! जिसमें सरकारी मोहर लगी होती है, वह क्या कहीं जाए, कहीं खाये, कहीं सोये, कहीं रहे कौन टोकने वाला है। मस्ताना वही है जिसने अपने व्यक्तित्व का, मानापमान का त्याग कर दिया है। जिसे अपने आप का भान भी नहीं है। जब तक अपने आपको कुछ न कुछ मानता है तब तक वह मस्ताना नहीं है। आत्म तत्व को जानने के लिये कुरबानी तो करना ही होता है। अपने व्यक्तित्व को गला देना होता है। चाहे जागे, चाहे सोवे, कोई क्या कहने वाला है।
खसम बिना जस राँड़, चाहे जागे चाहे सोवे ।
मन माना जग मुवा, भला अब किसको रोवे ।। 2 ।।
कहता 'मुक्ता' सत्य, मान बिनु जिसने जाना ।
हुआ निरंकुश पुरुष दीवाना मस्ताना ।। ३ ।।
बिना अपने आपको कुछ माने हुए जो आत्म तत्व को जानता है।
भया निरंकुश पुरुष दीवाना मस्ताना ।।
चलो, अब युक्ति जगत में भ्रमण करें। अभी तक शास्त्रोक्त प्रमाणों से सिद्ध किया गया और अब जरा युक्ति जगत में घूमें। देखो-शिव शिव सुनो- पहले जीववादियों का तर्क सुनो-
जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है ।
जीव अल्पशक्तिमान है, ईश्वर सर्व शक्तिमान है।
जीव छोटा है, ईश्वर बड़ा है।
जीव मृत्यु वाला है, ईश्वर अमर है।
जीव परिच्छिन्न है, ईश्वर व्यापक है।
जीव एक देशीय है, ईश्वर सर्वदेशीय है ।।
बिल्कुल ठीक-सोलह आने ठीक-परन्तु भैया ! (एक-एक फूल अलग- अलग हाथों में रखकर पू. श्री स्वामीजी समजा रहे हैं।)
जीव अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ ।
जीव अनेक, ईश्वर एक ।
जीव परिच्छिन्न, ईश्वर व्यापक ।।
तो इन दोनों को तौलने वाला, इन सबका परिज्ञाता फिर तीसरा कौन है, जो ईश्वर और जीव का वजन कर रहा है? तब तो दिखता है कि तौलने वाले को तौलना आता ही नहीं। अरे भाई! अपने को भी तराजू में रखकर तौलता है क्या? जीव और ईश्वर-बुद्धि रूपी तराजू के पलवे पर तुल रहे हैं। यदि मानों कि जीव तौल रहा है तो ईश्वर को जीव कैसे तौलेगा। एक आकाश का और एक जमीन का रहने वाला है, तो फिर तीसरा कौन है जो तौल रहा है? 'मैं' आत्मा । तीसरा तौलने वाला 'मैं' आत्मा ही हूँ। मुझमें ही ईश्वर और जीव दोनों कल्पित हैं। तो फिर यह जानता कौन है? इसका साक्षी कौन है? जीव अल्पज्ञ हैं और ईश्वर सर्वज्ञ है-इसका परिज्ञाता कौन है? 'मैं' आत्मा।
दूसरी युक्ति- एक जीव और दूसरा ईश्वर और तीसरा जीव और ईश्वर का भेद-बिल्कुल ठीक-भला बताओ-भेद का आधार कौन है? इस भेद को, इस तर्क को समझना है, यह लॉजिक है। यह भेद यदि ईश्वर में हो तो ईश्वर भेद रूप हो जाएगा। तो ईश्वर भेद रूप है कि अभेद रूप है? इस तर्क से ईश्वर। भेद रूप हुआ। तो बाबूजी ! भेद एक में होता है या दो में? ईश्वर एक है या दो? भेद का अस्तित्व ही दो में है और यदि ईश्वर भी दो होकर रहेगा तो यह अविनाशी नहीं। अर्थात् यदि ईश्वर भेद रूप है तो वह ईश्वर नहीं और ईश्वर यदि अभेद रूप है तो जीव और ईश्वर में भेद नहीं। ईश्वर से जीव का क्या, एक तृण का भी भेद नहीं है। यह ब्रह्मास्त्र है। इन्द्र का वज्र भले ही कुण्ठित हो जाय, परन्तु यह सिद्धांत कुण्ठित नहीं हो सकता। सब कुछ भगवान है-जीव भी भगवान है, जर्रा-जर्रा भगवान है। भगवान भेद रहित है अब कहाँ का द्वैत, विशिष्टाद्वैत-भेतवार्ता कथं भवेत्। सुनो, अब विचार करो-ध्यान दो, यहाँ कोई मजहबी, पंथ-पंथाई, साम्प्रदायिक चीज नहीं है-पंथ वाला नहीं, जो हकीकत है, सच्चाई है, सत्य है वही कही जाती है। सिद्ध करो भेद को-
यदि भेद रूप है तो वह ईश्वर नहीं, अभेद रूप है तो कण-कण (ईश्वर) है। सुई के अग्रभाग से भी भगवान अलग नहीं।
अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाह विच्क्ष्व भोः ।
न नौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि ।।
(श्रीमद्भागवत 4-28-62)
जो मैं हूँ वही तू है। जीवात्मा और परमात्मा में किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं है।
तावत् गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुकाः विपिने यथा ।
न गर्जति महाशक्तिर्यावद्वेदान्त केसरी ।।
जी हाँ- संसार रूपी जंगल के अनेकों मत मतान्तर रूपी सियार (लोमड़ी) कब तक चिल्लाते हैं जब तक कोई वेदांत रूपी सिंह की दहाड़ नहीं होती। संसार में अनेकानेक मत, पंथ-पंथाई, साम्प्रदायिकता आदि तभी तक पनपती है, भेदवादियों की चाल तभी तक चलती है, जब तक वेदांत सिंह की दहाड़ नहीं होती। तभी तक वे बोलते हैं। वेदांत केसरी, आत्मतत्व भगवान 'मैं' का रूप वेदांत रूपी तालाब में लखा देते हैं कि जानो तुम कौन हो-तुम्हें अपने आपका आत्मतत्व का, अपने 'मैं' का अनुभव करा देते हैं। यदि तुम विद्वान हो तो शास्त्रों का प्रमाण लो-उपनिषदों का, पुराणों का, स्मृतियों का, रामायण, गीता, भागवत आदि ग्रन्थों का प्रमाण लो और यदि तुम पढ़े-लिखे नहीं हो तो युक्तियों का प्रमाण लो और यदि तुम श्रद्धालु हो तो संत वाक्यों का प्रमाण लो, आप्त वाक्यों का प्रमाण लो। शरीर से भिन्न होकर, अपने आपको साढ़े तीन हाथ का न मानकर जब देखोगे तो फिर 'मैं' ही हूँ दिखेगा। हाँ, इस शरीर के अंदर जरूर हूँ, परन्तु शरीर दृष्टि छोड़कर समझना तभी आत्म तत्त्व का 'मैं' का अनुभव कर सकोगे। अनादिकाल से संसृति दोष से ग्रसित हो अपने आपको शरीर माने बैठे हो, इसी से यह असाध्य रोग हो गया है। इस अज्ञान को दूर करना ही होगा और फिर तो तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो ही। वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सभी इसी तत्व का प्रतिपादन करते हैं। हाँ वेद बड़ा और हनुमान चालीसा छोटी पुस्तक है। शरीर के अंदर रहते जो भगवान आत्मा 'मैं' अपना आप, जो जाहिर जहूर है, सब में निरंतर जो 'मैं' हूँ, 'मैं' हूँ की आवाज दे रहा है, इससे जो भिन्न है वह भगवान नहीं है। इस जिले का इस प्रान्त का यह पहला चांस है कि इस तरह अध्यात्म का प्रचार, डंका बज रहा है और यह डंका झंडापुर में ही सीमित नहीं है। झंडापुर तक ही नहीं है, वरन् सारे विश्व में गूंज रहा है। हम कथा प्रारंभ करते समय शांति पाठ के साथ ही घोषित कर देते हैं-अनन्त नाम, रूपों में अभिव्यक्त, अहमत्वेन प्रस्फुरित, महामहिम, स्वात्मस्वरूप सकल चराचर-यह ब्राडकास्ट यहीं के लिये नहीं वरन् सारे विश्व के लिए है ब्रह्मतत्व का प्रतिपादन (आत्म निरूपण) अध्यात्म विद्या है। याद रखो, वह दिन आज से दूर नहीं है, जबकि सारे विश्व में यह अध्यात्म विद्या ओतप्रोत हो जाएगी, कोना-कोना भर जाएगा। कहीं कोई स्थान खाली न रहेगा। ध्यान रहे कि यह अध्यात्म विद्या कोई पंथ या मजहबी चीज नहीं है। आजकल का समय प्रेक्टिकल एवं विज्ञान युग है। यह तो सभी को मालूम है कि विज्ञान जगत में कितनी प्रगति हो चुकी है और आगे बढ़ रही है। लोग चंद्रलोक की यात्रा कर चुके, वहाँ के धरती का फोटो लेकर यहाँ आए हैं और आगे वहाँ कोठी बनाकर रहने की तैयारी हो रही है और यहाँ अभी वही पुरानी रागिनी आलापी जा रही है। प्यारे ! प्रगतिशील बनो, अंधेरी ढोते जिंदगी बरबाद हो रही है। आलोक जगत में आओ-कब तक अंधकार में पड़े रहोगे। भेदवादियों के बीच पड़कर मन संकुचित हो चुका है। यह जीव का काम नहीं, यह नारायण का काम है कि जो हम तुम्हें घंटों उपदेश दे रहे हैं। अध्यात्म तत्व का अमृत तुम्हें पिला रहे हैं। यह तो हमारी सरकारी ड्यूटी है। घंटों आप लोगों को सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व बतला रहे हैं। हम इसलिए शरीर धारण किए हैं। हमें और कोई काम नहीं, बस एकमात्र यही चिंता है कि कितनी जल्दी तुम प्रकाश में आओ-अपने आप 'मैं' को समझ लो।
हाँ जी-क्या कोई कुछ पूछता है-स्वामी जी ! कहो भाई-स्वामी जी ! अगर हम जीव को ईश्वर का अंश मान लें तो क्या कोई हर्ज है? अपने आप को ईश्वर का अंश मान लें तो कोई हर्ज नहीं है और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी तो रामायण में यही लिखे हैं-
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखरासी ।।
(उ.कां.)
हाँ ठीक है, लिखा तो है भाई-तो फिर क्या चौपाई गलत है? क्या जीव ईश्वर का अंश नहीं है। इस ऊपर की चौपाई से तो साफ दिखता है कि जीव ईश्वर का अंश है। मेरे आत्मन् ! पूरी तरह समझकर अर्थ करो-पूरे पद पर गौर करो-आगे श्री गोस्वामी जी क्या कहते हैं-जीव ईश्वर का अंश है और फिर अविनाशी है-ईश्वर का अंश जीव अविनाशी। जीव का नाश नहीं होता, क्योंकि अविनाशी है-जीव मरता नहीं। तो फिर समझो, जीव अजन्मा होकर नहीं मरता कि जन्म लेकर नहीं मरता? यह तो अटल सिद्धांत है कि जो जन्म लेता है वह अवश्यमेव मरता भी है। जो जन्मेगा वह मरेगा भी। तो फिर इस तरह जरा-सा विचार करते ही जीव का जन्म-मरण टल गया और जो अजन्मा अविनाशी है उसे ही सत्य कहते हैं। वही सत्य होता है और आगे समझो जीव चेतन है कि जड़? नहीं जीव चेतन है। तब तो फिर जीव अविनाशी है और चेतन है-चित है और फिर जीव अमल है, शुद्ध आनंद स्वरूप है। जीव में मल (विकार) नहीं है। सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। जीव अमल है। सहज स्वाभाविक है, बनावटी नहीं। जीव सुख राशि है कि दुःख राशि? नहीं सुख राशि है। तो भैया ! हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। श्री गोस्वामी जी जो कहे हैं वही हम भी कह रहे हैं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखरासी ।।
हमने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं मिलाया है। हमारे प्रवचन में तुम यही पावोगे। हम उसी तरह से व्याख्या करेंगे जो भागवत, गीता, रामायण में दर्शाये गये हैं जो बात जैसी है, उसी तरह कहेंगे। यह बात अलग है कि गीत उसी के गाये जाते हैं जिसकी शादी होती है, चाहे दुल्हा काना हो या बहरा-आँख वाले के ही गीत गाते हैं ऐसा नहीं। तो उसी प्रसंग में प्रसंगानुसार शास्त्रों द्वारा अनुमोदित व्याख्या करता हूँ। यहाँ खींचातानी का अर्थ नहीं होता।
हाँ, तो विषय पर आ जाओ-जीव सोपाधिक है कि निरुपाधिक? जीव भाव सोपाधिक है, निरुपाधिक नहीं। अब देखो-जीव जब सत, चित, आनंद स्वरूप है तो ईश्वर अंश क्यों कहा? सुनो भैया ! यह जो अंशाशी भाव है वह सोपाधिक है, निरुपाधिक नहीं। अब जीव को सगुण ईश्वर का अंश कहें या व्यापक ईश्वर का अंश कहें। यदि जीव को सगुण का अंश मानो तो सगुण ईश्वर का अंश जीव साकार होगा, व्यापक नहीं। परिच्छिन्न होगा। साकार का टुकड़ा (जुज) भी साकार ही होगा। विज्ञान भी तो यही सिद्ध करना चाहता है, परन्तु जीव को आज तक कोई देख नहीं सका। जीव नजर नहीं आया। अरे ! यदि सूक्ष्म अंश ही मानो तो भी खुर्दबीन (माइक्रोस्कोप) से देख सकते हैं, परन्तु जीव दिखाई नहीं देता। तो फिर जीव सगुण ईश्वर का अंश नहीं और फिर जीव मानते हो अनेक। जीव अनेक हैं देखो- (पूज्य श्री स्वामी जी एक फूल लेकर एक-एक दल निकालते हैं।) जीव धड़ाधड़ निकल रहे हैं। तो कभी न कभी सगुण के अंश का भी अंत हो ही जाएगा, क्योंकि सगुण परिच्छिन्न होता है, सीमित होता है। इसलिए भी जीव सगुण ईश्वर का अंश नहीं सिद्ध होता। चलो-व्यापक ब्रह्म का खंड माने तो व्यापक निराकार में अंश भाव नहीं होता। तो फिर श्री गोस्वामी जी ने जीव को अंश कैसे लिखा? तो सुनो बात-
आत्मा ह्याकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवोदितः ।
घटादिवच्च संघातैर्जातावेतन्निदर्शनम् ।।
(माण्डू.गौ.का.अद्वै.प्र. 3)
देखो, थोड़ी देर के लिए मान लो यह (एक गिलास को दिखाकर कह रहे हैं।) एक घड़ा है। इसके अंदर का जो पोल है उसको कहते हैं घटाकाश। यदि दस घड़े हों तो दसों घड़ों में दस घटाकाश दिखाई देगा। आकाश की यह घटाकाश संज्ञा घट उपाधि से ही है। जैसा घट का रूप है वैसा ही उसका पोल आकाश-लम्बे में लम्बा, चौड़े में चौड़ा, गोल में गोल, दिखाई देता है। जो विस्तृत आकाश है वही आकाश इस घट में भी है। तो फिर ये आकाश दस नहीं है, एक ही है। आकाश, गोल, लम्बा, चौड़ा नहीं है। जैसा का तैसा बना बनाया है। यदि इसका खण्ड करना चाहो तो नहीं हो सकता। दरअसल में अंशाशी भाव आकाश में नहीं है। परन्तु घट मठादिक उपाधियों के कारण उसे घटाकाश मठाकाश आदि कहते हैं। इस घट उपाधि के कारण घटाकाश को आकाश का अंश मान सकते हैं। नहीं तो इसके अंदर का जो आकाश है, घटाकाश, वह कहीं से आया नहीं है और घट के फूट जाने से वह कहीं जाता नहीं।
घटादिवच्च संघातैर्जातावेतन्निदर्शनम् ।।
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चतुष्टय अन्तःकरण, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण इन संघातों को घटादि के समान ही समझना चाहिए। भगवान आत्मा आकाशवत है और घट रूपी संघात उपाधियों के कारण वह घटाकाश रूपी जीव चेतनांश कहा जा सकता है।
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा ।
आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि ।।
(माण्डू.गौ.का.अद्वै.प्र. 4)
जिस प्रकार घट के फूट जाने से घटाकाश महाकाश हो जाता है। इसी प्रकार शरीर के छूट जाने पर जीव साक्षात् परमात्मा हो जाता है। न कहीं जाता है और न कहीं से आया है। सच्चाई तो यह है कि घटाकाश संज्ञा घट से जब तक संबंध है तभी तक है, इसी तरह शरीरोपाधि तक ही जीवभाव है। अपने आपको ही अनेक जीव मान रहा है। जैसे दस घड़े का दस घटाकाश। परन्तु यह सब समय में ठीक नहीं है। जब तक अपने आपको साढ़े तीन हाथ का शरीर मानता है, इस मान्यता की परिधि में बंधा हुआ है, तभी तक शरीर में जीव की भिन्नता भास रही है। वस्तुतः आत्मा को शरीर से भिन्न करके जानो तभी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं। इसलिए वस्तुतः जीवभाव सोपाधिक है, निरुपाधिक नहीं। काल्पनिक है, वास्तविक नहीं।
सो मायावश भयउ गोसांई। बंधेउ कीर मरकट की नाई ।।
सो मायावश, कौन? अरे ! वही सोपाधिक घटाकाश रूपी जीव मायावश भयो। कैसे? जैसे-कीर (तोता और मरकट बंदर)। तोता कैसे फँसता है?
जंगलों में तोता फँसाने वाला बहेलिया इस झाड़ से उस झाड़ तक एक लम्बी रस्सी बांध देता है और उस रस्सी में बाँस की पोली पोंगरी (जैसे पंखों में घुमाते हो) पिरो देता है। फिर तोते को लालच देने के लिए पोंगरी के ऊपर तोते के खाने के लिए चारा रख देता है ताकि तोता उसे देखकर खाने के लिए पोंगरी पर बैठे। तोता जब खाने के लिए जाता है और पोंगरी पर बैठता है तो उसके ही वजन से पोंगरी घूम जाती है और गिरने के डर से पोंगरी को मजबूती से पकड़ा तो, तोता उल्टा लटक जाता है। तोते के पकड़ते ही पोंगरी घूम जाती है और तोता समझता है कि पोंगरी ने उसे पकड़ रखा है। ध्यान दो-पोंगरी तोते को क्या पकड़ेगी। वस्तुतः उसने ही स्वयं पोंगरी को पकड़ रखा है। पोंगरी जड़ है और तोता चेतन, उसे भला जड़ पोंगरी क्या पकड़ेगी। बस, यही मान्यता, कि पोंगरी ने उसे पकड़ लिया है, उसके बंधन का कारण है। वह लटका रह जाता है और इस तरह बहेलिए के हाथ आ जाता है।
देखो बंदर का हाल-जहाँ पर ज्यादा बंदर होते हैं, वहाँ पर बंदर पकड़ने वाले कुछ दूरी पर दस-बारह सुराही जिसमें आधे दूर तक चने भरे होते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। चूँकि सुराही का गला सकरा होता है बंदर की भरी मुट्ठी बाहर नहीं निकलती। (अब पू. श्री स्वामीजी बंदर का स्वांग बनाते हैं) - अब बंदर आया इधर-उधर चारों तरफ देखकर सुराही के पास धीरे से जाता है और चना देखकर खाने की लालच से चना निकालने के लिए सुराही के अंदर हाथ डाल देता है, क्योंकि सुराही के अंदर बंदर का ही हाथ जा सकता है, हमारा तुम्हारा नहीं। अब देखो, मुट्ठी में चना भरा है और हाथ बाहर निकालने के लिये वह भरसक कोशिश करता है, परन्तु सुराही का मुंह छोटा होने की वजह से ऊपर खींचने से हाथ नहीं निकलता, अटका रह जाता है। इस तरह बंदर समझता है कि सुराही ने उसे पकड़ रखा है। बंदर क्या देखता है कि हाथ नहीं निकल रहा है, अंदर से बंदर की मुट्ठी चने से भरी बंधी है-नहीं निकलती-सीधा हाथ रखता तो निकल जाता। जब हाथ नहीं निकलता तो बंदर
समझता है कि सुराही ने उसे पकड़ लिया है। अब सुराही जड़ है और बंदर चेतन। तो चेतन बंदर को जड़ सुराही क्या पकड़ेगी।
आपन तो आपन ही विसर्यो ।
जैसे श्वान काँच मंदिर में, भ्रमि-भ्रमि चौंकि मरयो ।।
मर्कट मूठि छाड़ि नहिं दीन्हीं, घर-घर द्वार फिर्यो ।
सूरदास नलिनी को सुवटा, कहु कौने पकर्यो ।।
आपन को आपन ही विसर्यो ।
आप भुलान्यो आपमें, बन्धेउ आप ही आप ।
जाको ढूँढ़त फिरत है, सो तू आप ही आप ।।
अपने आप फँसा हुआ है। देखो, कोई सज्जन आये हैं-प्रश्न हो रहा है- साहब! आप आये नहीं? स्वामी जी ! मैंने तो सुना जरूर है कि आपका यहाँ वेदांत पर प्रवचन हो रहा है और मेरी इच्छा भी सुनने को हुई, परन्तु क्या कहें ऐसा जंजाल है-मैं तो माया के चक्कर में पड़ा हूँ-
चालीस वर्ष के अनवरत प्रचार में हमने यही देखा है-लोग कहते हैं कि माया के चक्कर में पड़ा हूँ। कोई नहीं कहता कि माया राँड़ मुझे पकड़ी है, चक्कर में डाल रखी है। अरे! भीतर वाला सत्य सनातन ब्रह्म कभी झूठ नहीं बोलता। अंदर वाला सत्य ही कहता है। मैं स्वयं अपने आप माया के चक्कर में पड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे माया के चक्कर ने डाल रखा है। तो भैया ! बताओ, किसने तुमको कहा कि तुम माया के चक्कर में पड़ो? तुम स्वयं ही माया के चक्कर में पड़े हो। तुम अपने ही संकल्प से बंधे पड़े हो। कोई तुम्हें बांधा नहीं है। तोताराम को संत यही उपदेश देते हैं कि ऐ बेटा गंगाराम ! तू चेतन है और पोंगरी जड़ है, तुझे पोंगरी क्या पकड़ेगी। तू स्वयं पोंगरी को पकड़ा है, पोंगरी तुझे नहीं पकड़ी है, उड़ जा-पोंगरी को छोड़ दे। यदि इस महामंत्र को तोता ने मान लिया तो उसका उद्धार हो गया, नहीं तो लटका तो है ही। वैसे ही बंदर के लिए यही उपदेश है कि तू स्वयं मुट्ठी बांधकर पड़ा है, सुराही तुझे नहीं पकड़ी है, मुट्ठी खोलकर भाग जा। संत महात्माओं द्वारा यही आत्मतत्व का उपदेश है कि बेटा! तू आत्मा है, देह भाव को छोड़ दे और अपने स्वरूप 'मैं' (आत्मतत्व) को जान, इस गलतफहमी देहभाव को छोड़कर स्वस्वरूप भगवान आत्मा 'मैं' को जानो, पहचानो। तीन काल में जन्म, मरण नहीं है। आवागमन के चक्र से बाहर आओ। इस भ्रमण को बंद करो और अपने नारायण स्वरूप में जागो-नहीं तो फिर पड़े रहो।
समझो, तुम सर्व के आधार हो, गुरुजन, विद्वज्जन, आत्मतत्व का अनुभव कराते हैं। यदि समझ गया तो फिर यही मोक्ष है। अरे! जब बंधा ही नहीं है तो उससे मोक्ष कैसा-जीव का बंधन यदि सत्य है तो इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती और यदि असत्य है तो है ही नहीं फिर मोक्ष होगा किससे? अपने आपको जीव या कुछ भी मान लेना यही बंधन है और अपने आपको 'मैं' आत्मा जान लेना यही मोक्ष है।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।।
(गीता 6-5)
संत महात्मा उपदेश देते हैं-अरे भाई ! यह उनकी ड्यूटी है। संत तो तुम्हें अपने 'मैं' का, आत्मतत्व का अनुभव करा देंगे-तुम्हें लखा देंगे-विचार करता है तो ठीक है। जानना, न जानना तुम्हारा काम है।
नानक निदरी निदर निहाल ।
क्या देरी है, मुक्त हो जा। हृदय में भूख तो लगे, आत्म तत्व को जानने की प्रबल जिज्ञासा तो जगे वैसे तुम स्वयं आत्मस्वरूप ही हो, अपने आप को ही जीव मानकर कष्ट पा रहे हो। इस तरह उस वैदर्भी रानी जो कि पूर्वजन्म का राजा पुरञ्जन ही है, उसका अविज्ञात सखा, स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म प्रतिबिम्ब और बिम्ब के माध्यम से घटाकाश, मठाकाश द्वारा जीव का भ्रम मिटा देता है। जीव और परमात्मा (ब्रह्म) दोनों एक ही तो हैं।
---------
तृतीय दिवस
प्रह्लादोख्यान जीवन का लक्ष्य, आनंद की प्राप्ति गृहस्थाश्रम आत्मपात एवं अंधकूप है, उपासना ज्ञान भक्ति
।। श्री नारायणोपनिषत्पाठ ।।
अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा-दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम् ।
विविधविषय धर्मग्राहिमुग्धेक्षणानांप्रणतभयविहन्तृ ब्रह्म यत्तन्नऽस्मि ।।
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम् ।
देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ।।
मूकं करोति वाचालं पङ्कलङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम् ।।
अनन्त नाम, रूपों में अभिव्यक्त, अहमत्वेन, प्रस्फुरित, महामहिम, स्वात्मस्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित आत्म जिज्ञासुगण !
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्निबोधत ।।
अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वालों भव्य जीवों ! उत्तिष्ठत- उठो। स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो, किसी श्रेष्ठ महापुरुष के सान्निध्य में उपसन्न होकर अपना आत्म कल्याण करो। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता के माध्यम से आत्मतत्व का निरूपण हो रहा है। कल के प्रसंग में कर्मों की विवेचना सुने हो। राजा पुरञ्जन के आख्यान में जीव और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित की गई थी। आज का प्रसंग है प्रह्लादोपाख्यान -
किसी समय दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने दैत्यों की महती सभा बुलाकर उन्हें सावधान किया। उन्हें संबोधित किया कि ऐ दैत्यों ! तुम लोग मेरी बात सुनो- भगवान विष्णु ने वनचर वाराह का रूप धारण कर हमारे परम प्रिय हितैषी छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया है और अभी तक मैंने उसका तर्पण श्राद्ध भी नहीं किया है। अतः, मैंने निश्चय किया है कि मन्दराचल पर्वत की कन्दरा में जाकर परमेष्ठी भगवान ब्रह्माजी को कठिन से कठिन तप करके संतुष्ट करूँगा। तप सिद्ध हो जाने के बाद भगवान विष्णु से युद्ध करूँगा। युद्ध में उनका शिरच्छेदन करके उसी के रुधिर की धारा से मैं अपने परम प्रिय भाई के नाम से तर्पण करूँगा। यहाँ पर तुम लोग सावधानी से राज्य और कुटुम्बियों की रक्षा करना। हो सकता है कि मेरे तप के लिए जाने के बाद देवता लोग यहाँ आकर उपद्रव करें, तो तुम लोग डटकर उनका सामना करना। तप से उठने पर मैं उन सबको देख लूँगा। इस तरह सभी दैत्यों को सावधान करके हिरण्यकश्यप तप करने मंदराचल पर्वत की तरफ चला गया।
स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमादारुणम् ।
उर्ध्वबाहुर्नभोदृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः ।।
(श्रीमद् भागवत 7/3/2)
हिरण्यकश्यप मन्दराचल पर्वत की कन्दरा में जाकर महान दारुण तप करने लगा। वह अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर और आँख को आकाश की ओर उठाकर अपने दाहिने पैर के एक अंगूठे के भार से खड़ा होकर दारुण दुःखदाई तप करने लगा। इसी तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। इस दारुण तपस्या से अंतरिक्ष में चारों तरफ आग की भीषण ज्वाला निकलने लगी और वह ज्वाला दसों दिशाओं में फैल गई। समुद्र का जल उबलने लगा। आकाश से तारे टूट-टूटकर गिरने लगे। पृथ्वी डगमगाने लगी। संसार में हाहाकार मच गया। जब अग्नि की ज्वाला देवलोक तक पहुँची तो देवता भी जलने लगे और वे बहुत घबरा गए। इन्द्र इस विप्लव से डर के मारे सभी देवताओं को लेकर ब्रह्माजी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभो! इसके तप से स्वर्ग लोक एवं सारी पृथ्वी दग्ध हो रही है। आपकी बनाई सारी सृष्टि न रहेगी। आप से हम सभी देवता प्रार्थना करते हैं कि हिरण्यकश्यप के उग्र तप को शांत कीजिये। देवताओं द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर परमेष्ठी ब्रह्माजी हंसवाहन पर आरुढ़ हो भृगु आदि ऋषियों को लेकर जहाँ हिरण्यकश्यप तप कर रहा था, पहुँचे। परन्तु, जहाँ हिरण्यकश्यप तप कर रहा था, वहाँ पहुँचने पर हिरण्यकश्यप कहीं दिखाई नहीं दिया।
न ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकैः ।
पिपीलिकाभिराचीर्णमेदस्त्वङ्गासशोणितम् ।।
(7/3/15)
वहाँ पर वल्मीक (बॉबी) में उसका शरीर छिप गया था। मिट्टी, घास, तृण आदि से हिरण्यकश्यप का शरीर आच्छादित हो गया था और अंदर से चीटियाँ उसके मेदा, त्वचा, मांस, शोणित सब चाँट गई थीं। केवल अस्थि पिञ्जर मात्र शेष रह गया था।
विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्हंसवाहनः ।।
(7/3/16)
उसको देखकर ब्रह्माजी भी महान विस्मित हो गए। उन्होंने हँसते हुए कहा-अरे !
उत्तिष्ठोतिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोसि काश्यप ।
वरदोऽहमनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः ।।
(7/3/17)
महर्षि कश्यप के पुत्र हे काश्यप ! उठो, उठो बेटा। तुमने तो मुझे भी जीत लिया। विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा उग्र तप किसी ने नहीं किया।
नैतत्पूर्वर्षयश्चकुर्न करिष्यन्ति चापरे ।
निरम्बुर्धारयेत्प्राणान्को वै दिव्यसमाः शतम् ।।
(7/3/19)
तुमने देवताओं के सौ वर्ष तक बिना जल के तप किया है। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। इस तरह देवताओं के सौ वर्ष तक तूने उग्रतप किया है। अन्न के बिना प्राण रह सकता है, परन्तु जल के बिना नहीं रह सकता। प्राण को रोकने के लिए जल परमावश्यक है।
ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव ।
मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम् ।।
(7 - 3 - 21)
उठो, उठो और अपना अभीष्ट वर मांग लो, ऐसा कहकर ब्रह्माजी ने अपने कमण्डल से दिव्य एवं अमोघ जल लेकर उस बॉबी पर मार्जन किया। छींटा दिया।
कमण्डलुजलेनौक्षद्दिव्येनामोघराधसा ।।
(7 - 3 - 22)
तो वह हिरण्यकश्यप उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर सारा अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाये हुये सोने की तरह चमकीला दिव्य हो गया। वह ब्रह्माजी की स्तुति करने लगा-
नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये ।
प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारैव्र्व्यक्तिमीयुषे ।।
(7 - 3 - 28)
स्तुति के बाद वह वर मांगता है-
यदि दास्यस्यभिमतान्वरान्मे वरदोत्तम ।
भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्योमृत्युर्मा भून्मम प्रभो ।।
(7 - 3 - 35)
नान्तर्बहिर्दिवानक्तमन्यस्मादपि चायुधैः ।
न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि ।।
(7 - 3 - 36)
व्यसुभिर्वाऽसुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः ।
अप्रतिमद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम् ।।
(7 - 3 - 37)
सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथाऽऽत्मनः ।
तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कर्हिचित् ।।
(7-3-38)
वह वरदान मांगता है कि हे वरदोत्तम ! यदि आप मुझे मेरा अभीष्ट वर देने आये हो तो सुनो-आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी, मनुष्य हो या देवता मेरी मृत्यु न हो-यह पहला वर मांगा। न भूमौ नाम्बरै मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। न मैं पृथ्वी में मरुं न आकाश में, न दिन में मरूँ न रात्रि में, मनुष्य से मरूँ न पशु सिंह आदि से। त्रिलोकी का एकमात्र राजा होऊँ। युद्ध में मेरे सामने कोई खड़ा न हो सके। भगवन् ! यदि आप मेरा अभीष्ट वर देने आये हो तो यही दो। ब्रह्माजी विचार में पड़ गए। कुछ देर सोचने लगे-बड़ा कठिन वर मांगा है।
ततो जगाम भगवानमोघानुग्रहो विभुः ।
पूजितोऽसुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः ।।
(7 - 4 - 3)
भैया ! आज तक ऐसा कठिन वर किसी ने भी नहीं मांगा जैसा दुर्लभ वर तुमने मांगा है। अच्छा-जाओ, मैंने तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट वर दे दिया। ब्रह्माजी वर देकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। हिरण्यकश्यप ऐसा उत्तम वर प्राप्त कर अपनी राजधानी को न लौटकर सीधे स्वर्ग लोक (अमरावती, देवलोक, इन्द्रपुरी) को जा पहुँचा। वहाँ क्या देखता है कि देवता सभी देवलोक छोड़कर पहिले से ही भाग गए हैं, इंद्रासन खाली है। हिरण्यकश्यप इन्द्रासन पर बैठ गया और गंधर्व विश्वासु, तुम्बर, किन्नर, विद्याधर एवं अप्सरायें हिरण्यकश्यप का गुणगान करने लगे। अरे! हाँ गंधर्व, किन्नर उसका गुणगान क्यों न करें, यह उसका तपोबल है, तपश्चर्या का फल है-गवर्नमेंट ही जब बदल गई। पृथ्वी उसके भय के बिना जोते-बोये ही अन्न पैदा करने लगी। समुद्र रत्नों को बहाकर किनारों पर ढ़ेरी लगा देने लगे। पर्वत अपनी घाटियों के सुरम्य स्थान उसके आखेट खेलने के लिए जुटा देने लगे। वृक्ष सब ऋतुओं में फूलने-फलने लगे यह सब ऐश्वर्य तप के प्रभाव के हिरण्यकश्यप को प्राप्त हो गया। इन सब ऐश्वर्यों (भोगों) को भोगकर भी, यह सब होने पर भी-
यथोपजोषं भुञ्जानों नातृप्यदजितेन्द्रियः ।।
(7 - 4 - 19)
अजितेन्द्रियः हिरण्यकशिपुः न तृप्येत्। यह सब कुछ प्राप्त होने पर भी उसकी तृप्ति न हुई। स्वर्ग के कल्पवृक्ष, कामधेनु, अमूल्य रत्न चिंतामणि आदि वैभव प्राप्त कर लेने पर भी, पृथ्वी और देवलोक का सारा सुख वैभव करतलगत होने पर भी तृप्ति नहीं हुई। अब विचार करना है कि इतना ऐश्वर्य (रिद्धि, सिद्धि) पाने के बाद भी तृष्णा क्यों शांत नहीं हुई? मन की भूख, मन की तृष्णा, शांत क्यों नहीं हो? कहते हैं-
निस्स्वोद्रव्यशतीशतं दशशताम् सोऽपीह लक्ष्येशताम्,
लक्ष्येशः क्षितिराजतां क्षितिपतिस्चक्रीधरत्वम् पुनः ।
चक्रीमः सुरराजतां सुरपदंब्रह्मास्पदं वाञ्छति,
ब्रह्मा विष्णुपदं हरिस्शिवपदं तृष्णावधिं को गतः ।।
चाहे वह सुरपद, ब्रह्मपद को भी क्यों न पा ले, वह शिवपद को भी चाहे क्यों न प्राप्त कर ले, तृष्णा शांत नहीं होती, वह संतुष्ट नहीं होता। किसी के पास एक भी रुपया नहीं है उसे यदि एक रुपया मिल जाए तो फिर उसे तृष्णा पैदा होती है कि उसे सौ रुपये मिल जाये। यदि उसे वह भी मिल जाता है तो वह हजार की प्राप्ति की इच्छा करता है। फिर लाख और करोड़पति बनना चाहता है। तृष्णा यहीं शांत नहीं होती। तब फिर वह राजा बनूँ, चक्रवर्ती बनूँ, सम्राट कहाऊँ, मुझे देवराज इन्द्र का सिंहासन मिले, ब्रह्म पद, शांकर पद, विष्णु पद पाने की इच्छा करता है। परन्तु, यदि वह इन्हें भी प्राप्त कर ले तो भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तो फिर देखें, इस प्रश्न पर विचार करें कि तृष्णा कैसी बलवती है और कभी तुष्ट क्यों नहीं होती। चलो, विचार वाटिका में भ्रमण करें-देखो मन क्या चाहता है? मन की भूख क्या है? मन की तृष्णा, मन की आकांक्षा क्या है। बताओ, हर एक के मन की चाह क्या है? मन अनादिकाल से क्या चाहता है? देखो दस, पाँच आदमी मनोविनाद के लिए आपस में चर्चा करते हैं कि भाई! हम लोग संसार में आये हैं तो इस संसार में हमारा क्या कर्तव्य है? हमें क्या करना चाहिए?
यदि उस गोष्ठी में, उस समाज (मंडल) में कोई संन्यासी बैठा हो तो वह कहेगा कि संसार असार है, मिथ्या है कहीं जंगल में जाकर भगवान का भजन करना चाहिये। वह वैराग्य की महिमा बताएगा। सब को त्याग कर संन्यास ग्रहण करना ठीक कहेगा। यदि उस समाज में कोई देशसेवक होगा तो वह कहेगा कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए और उसमें कोई चार्वाक का अनुयायी होगा, यदि उसका चेला होगा तो कहेगा-
न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।
नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ।।
यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वाघृतं पिवेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।।
भारत में चार्वाक नाम का एक बड़ा भारी नास्तिक हुआ है। उसका मत चार्वाक दर्शन है। वह कहता है कि यहाँ क्या करना है, जब तक संसार में जियो सुख पूर्वक जियो। यदि पैसा न हो तो ऋण लेकर घी पियो। अरे! देना तो है ही नहीं। 'ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।' शरीर के नाश होने पर कौन कहाँ आता-जाता है। नाशवान देह का कभी कहीं कोई आवागमन नहीं, वरन् शरीर मरने से नष्ट हो जाता है। 'न स्वर्गो नापवर्गों वा नैवात्मा पारलौकिकः' न आत्मा है न परमात्मा है। इस गोष्ठी में क्या भजन, क्या भाव। खैर यह बहुमत हो गया है। मौलिक प्रश्न तो यही है कि मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है? संसार में जन्म लिये हैं तो यार। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मनुष्यत्व क्या है? तो भैया! यह मौलिक एवं सार्वभौम प्रश्न है और उसका उत्तर भी मौलिक एवं सार्वभौम ही होना चाहिए। जन्म से लेकर मरण पर्यन्त मनुष्य जिस वस्तु को ढूँढ़ रहा है? उसे प्राप्त कर लेना, यही मनुष्यमात्र का कर्तव्य है। तो क्या ढूँढ़ रहा है? किसी से भी पूछो सभी एक स्वर में कहेंगे कि मनुष्य की खोज आनंद के लिए है। उसे आनंद चाहिए। किसी से भी पूछो, क्या वह आनंद का वैरागी है? नहीं, सभी को आनंद चाहिए। प्रपंच के वैरागी तो बहुत मिल जायेंगे, परन्तु सुख का वैरागी, आनंद का वैरागी तो कोई विरला ही होगा। कोई न मिलेगा जिसे कि आनंद से वैराग्य हो। जिस चीज की अनादिकाल से निरंतर तलाश हो रही है वह है आनंद की प्राप्ति। यहाँ पर आप लोग इतनी दूर से क्यों आये हो? हजारों मील से यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हो? इसलिए कि स्वामी जी का सत्संग होगा, दर्शन होगा-स्वामीजी के दर्शन के लिए आये हो-तो भैया! आनंद ही का लक्ष्य करके तो आये हो? लक्ष्य तो सबका एक ही है, मगर साधन में भिन्नता है।
मनुष्य ही आनंद चाहता हो, ऐसी बात नहीं है। पशु, पक्षी, कीट पतंग सभी आनंद चाहते हैं। सभी इसके ही लिए कार्य करते हैं कि हमें आनंद मिले। बिल्कुल ठीक। प्राणिमात्र का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। संसार में सभी प्राणी नैतिक-अनैतिक कार्य आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। मनुष्य मात्र संसार में जीवन के लिए नहीं जीता, उसे संसार जीने के लिए प्रिय नहीं है, आनंद मिलता है इसलिए प्रिय है। यही कारण है कि संसार उसे प्रिय है और आनंद नहीं मिला तो वही संसार बोझ रूप हो जाता है। प्राणिमात्र के जीवन का लक्ष्य आनंद ही है। आनंद ही उसका स्वरूप है। जिसके बिना जो एक क्षण भी न रहे, वही उसका स्वरूप होता है। मनुष्य आनंद के बिना, जीवमात्र आनंद के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। आनंद न मिले तो वह जहर खा लेगा। आत्महत्या पर उतारू हो जाता है। आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। आनंद का वियोग क्षणभर के लिए भी नहीं सह सकता। यदि मन का स्वरूप दुःखरूप होता तो वह दुःख को ही ढूँढता। बिना आनंद के वह जिंदा रहता। मछली का आधार उसका घर, उसका स्वरूप जल ही है। मछली जल स्वरूप ही है इसलिए जल के वियोग में मछली जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार मन की खुराक आनंद ही है। इसके बिना वह जी नहीं सकता। अनादिकाल से उसे आनंद ही की तलाश है। बस देखो-एक योगी पर्वत की कन्दरा में महान से महान कष्ट सहन कर घोर तप करता है, उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए दूसरा व्यक्ति घोर पाप करता है। किसलिए? आनंद की ही प्राप्ति के लिए। हाँ, लक्ष्य तो एक ही है, साधन भिन्न अवश्य है। जिस आनंद को ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य में ढूँढ़ता है। गृहस्थी उसी आनंद को स्त्री-पुत्रादिक में खोजता है। वानप्रस्थी तप द्वारा उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। संन्यासी उसी आनंद को संन्यास में ढूँढ़ता है। लक्ष्य सबका एक ही है, आनंद की प्राप्ति। पिता अपने नन्हे शिशु को गोद में बिठाकर उसके कोमल कपोलों पर बार-बार चुंबन करता है, प्यार करता है। इस प्यार में उसके मूँछ और दाढ़ी के कड़े बाल बालक के कोमल कपोलों में चुभते हैं, तो बालक रोता है, परन्तु पिता को मजा आता है। यह आनंद पिता के लिए है न कि पुत्र के लिए। इसी तरह जीवमात्र अनेकानेक साधनों में आनंद को ही खोजते हैं। कई एक को तो दूसरों की निंदा करने में ही मजा आता है-आनंद की प्राप्ति में यह भी एक साधन है। कभी-कभी जब लोग रोते हैं तो उसमें भी आनंद का अनुभव करते हैं। इस समाज में (प्रकृति समाज की तरफ इशारा करते हैं।) जब दो औरतें (स्त्रियां) आपस में मिलती हैं, तो तीसरी भी रहती हैं। हाँ कंधा बदलने के लिए, तो आपस में आनंदाश्रु बहाते हैं, रोते हैं। इसी तरह जब रोते भी हैं तो आनंद के लिए। न आनंद आये तो रोना बंद कर दें। हाँ-रोने में भी आनंद है। गरज तो यह है कि अनादिकाल से जीवमात्र आनंद ही ढूँढ़ रहे हैं। समस्त जीव किस तरफ बह रहे हैं? आनंद सागर की तरफ। अब विचार करना है कि जब आनंद की प्राप्ति के लिए सभी व्याकुल हैं, आनंद का स्रोत क्षण भर भी बंद न हो यही सबकी ख्वाहिश है, फिर भी आनंद की प्राप्ति उसे क्षणिक ही हो रही है। उसकी तृप्ति नहीं होती। जब क्षण प्रतिक्षण विषयों द्वारा आनंद मिलता ही रहता है तो फिर उस आनंद की प्राप्ति के बाद मंजिल खतम हो जानी चाहिये। मन की दौड़ खतम हो जानी चाहिए। परन्तु एक विषय के बाद दूसरे विषय में इस प्रकार नाना विषयों के तरफ मन दौड़ रहा है, अभी तक मंजिल तय न कर सका। अरे। जब तृप्ति नहीं होती तो वह सुख-सुख नहीं है। समझ लो-वह सुख-सुख ही नहीं जिसमें दुःख है, डर है और रोना है। स्त्री की प्राप्ति में दुःख है, मर न जाय इसका डर है और मर जाये तो रोना है। पुत्र की प्राप्ति में दुःख है, उसे कोई बीमारी न आ जाये, इसका डर है और निधन में रोना है। धन की प्राप्ति में दुःख है, कहीं खो न जाये, लुट न जाये, चोरी न हो जाय इसका डर है और लुट गया तो रोना है।
वह सुख सुख ही नहीं जिसमें दुःख है, डर है और रोना है।
मिलावट से जो है खाली उसी का नाम सोना है।
अरुण पर फेंक दो तुम धूल अंधियारा नहीं होता ।
करो तुम चूर्ण हीरों को मगर काला नहीं होता ।।
प्यारे ! वह सुख-सुख नहीं है, धोखे में न पड़ो, जिसमें दुःख है, डर है, रोना है। यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो फिर विचार करो वह कौन-सा सुख है, आनंद है जिसके लिए समस्त प्राणिवर्ग भटक रहे हैं? जिसे पाने के लिए अनादिकाल से चेष्टा हो रही है? क्या किसी को ऐसी इच्छा होती है कि 23 घंटा 59 मिनट तो आनंद भोगे, परन्तु यदि एक मिनट दुःख भोगने को मिले तो कोई बात नहीं है? ऐसी इच्छा किसी को भी नहीं होती। वह तो चौबीसों घंटे आनंद ही आनंद चाहता है। एक मिनट का भी दुःख ग्रहण करना नहीं चाहता। वह आनंद सागर चाहता है। प्रार्थना करता है कि हे भगवान ! हमारे सब दुःख दूर हो जायें, जीवन सुखमय आनंद से बीते। तो शाश्वत आनंद ही प्राणिमात्र का लक्ष्य है और शाश्वत आनंद ही प्राणि मात्र की खुराक है। जीव क्षणिक आनंद नहीं चाहता, वह नित्यानंद चाहता है। अरे भाई ! आनंद आया और चला गया, मन को तो संतोष हुआ ही नहीं। जहाँ एक विषय में मनीराम को कुछ आनंद मिला तो वह तुरंत ही दूसरे विषय में आनंद की फिराक में पड़ जाता है। तो फिर समझ लो कि यह सुख नहीं है जिसकी खोज मन को है। यह नित्यानंद ढूँढ़ रहा है। परन्तु विषयों में उसे क्षणिक आनंद ही मिल पाता है। इसलिए अनादिकाल से संसार भर में सभी की यात्रा नित्यानंद के लिए ही हो रही है। आज से नहीं, पता नहीं कब से, अनादिकाल से संसार की महान यात्रा शाश्वत आनंद नित्यानंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए है और समझ लो खूब ध्यान देकर कि आवागमन का चक्र मिटने वाला नहीं है जब तक कि वह अपने लक्ष्य नित्यानंद को प्राप्त न कर ले लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आवागमन का चक्र खतम होगा। जहाँ के लिए यात्रा हो रही है, जहाँ तुम जा रहे हो वह आखिरी मंजिल तुम्हारा घर हीहै, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। यहाँ पर तू-तू, मैं-मैं, ऊँचा-नीचा, गृहस्थी-वैरागी, चोर-जुआरी का प्रश्न नहीं है। क्या संन्यासी, क्या वैरागी सभी ढूँढ़ रहे हैं। इसी की प्राप्ति के लिए पुण्यी और पापी सभी को तलाश है। सभी के जीवन का लक्ष्य आनंदसागर (नित्यानंद) की प्राप्ति है। जिस समुद्र की प्राप्ति के लिए गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि समस्त नदियों की यात्रा हो रही है वहीं को गंदी नाली भी जा रही है। गंगा आदि समस्त पवित्र नदियों का जो घर है, वही घर गंदी नालियों का भी है। दोनों के घर में भेद नहीं है। इसी तरह जो नित्यानंद घर (चरम लक्ष्य) एक संन्यासी विरक्त महात्मा का, ब्राह्मण का है, वही नित्यानंद घर स्वपच, महान पापी, वज्र मूर्ख का भी है। जी हाँ-उसी को प्राप्त करना है। चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या यहूदी मनुष्य को कौन कहे, कूकर, सूकर इत्यादि सभी जीवमात्र का लक्ष्य है नित्यानंद की प्राप्ति। चाहे इसकी प्राप्ति एक जन्म में हो या अनेक जन्मों के बाद। लक्ष्य यही रहेगा। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा अभीष्ट नित्यानंद ही है। चाहे अनेकों जन्मों तक ढूँढ़ो लेकिन अंत में यही हल निकलेगा कि हम तो आनंद चाहते हैं। तब तक उसे विश्राम नहीं जब तक शाश्वत आनंद की प्राप्ति न हो जाए? आनंद का कहीं भी कोई वैरागी नहीं होता। जब सभी का लक्ष्य आनंद सागर है तो आपस में छोटा बड़ा कैसा? आपस में यदि नदियाँ लड़े कि हम बड़ी हैं, तुम छोटी हो, हम पावन हैं, तुम मलिन हो तो यह उनकी नासमझी होगी। जब उन सबकी यात्रा एक ही घर की ओर है। विचार करें तो सभी सागर की ओर जा रही हैं। गंगा और गंदी नाली सभी की पहुँच समुद्र के ही लिए है। नदियाँ सागर में (अपने घर, अपने विश्राम स्थल में) पहुँचने के पहले ही नाम, रूप की मान्यताओं का त्याग कर देती हैं। सभी नाम, रूप को छोड़ जल दृष्टि से एक ही हैं। इसी प्रकार शरीरों में भेद है, न कि अंतिम लक्ष्य में। भले ही हम सब शरीर दृष्टि से अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं, परन्तु आंतरिक दृष्टि से भैया। हम सब तो एक ही हैं। इस सत्य को समाज, देश एवं सारे विश्व को समझना होगा। इसके बिना एकता स्थापित नहीं की जा सकती। ध्यान रहे कि कानून से समाज में एकता स्थापित नहीं की जा सकती। समाज में एकरूपता नहीं होगी चाहे कानून राजनैतिक हो या सामाजिक। आज ऐसी क्रान्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसी क्रान्ति होनी ही होगी। भला बताओ, अरे। शरीर की भी एकता हुई है। चाहे कुछ समय के लिए एकता भले ही हो जाए, परन्तु वह टिकाऊ न होगी।
भाई। जो एक है वही एक होगा। जो अनेक है, उसमें तुम एकता चाहते हो? यह कैसे संभव होगा? तो जरूरत है इसी की, राष्ट्र को इसकी परम आवश्यकता है। घर-घर में इस सत्य को पहुँचाना होगा कि जीवमात्र नित्यानंद को ही ढूँढ़ रहा है। नदियाँ, समुद्र में पहुँचकर ही पूर्ण विश्राम पाती हैं। यह तो सिद्ध हुआ कि प्राणिमात्र की आखिरी मंजिल नित्यानंद की प्राप्ति है।
सरिता जल जलनिधि महँ जाई ।
होई अचल जिमि जिव हरि पाई ।।
देखिये, नदियों का बहना कभी बंद नहीं होता। वह बंद होता है, समुद्र की प्राप्ति के ही बाद। इसी तरह जीव कहो या मन कहो ये पर्यायवाची शब्द हैं। जीव का आवागमन ब्रह्मानंद की प्राप्ति के बिना बंद नहीं होता, भ्रमण चलता ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था (गाढ़ी नींद) में अज्ञान में जब मन का लय हो जाता है, उस स्थिति में मैं जीव हूँ-यह भाव भी नहीं रहता। मन सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में लीन होता है। मूर्छावस्था में मन दुःख में लीन होता है और समाधि में चेतन आत्मा में लीन होता है। जब मन नहीं रहता तो मैं जीव हैं-यह भाव भी नहीं रहता। जब तक मन का अत्यन्ताभाव नहीं होता, अमन नहीं होता, आत्म भाव में लीन नहीं होता तब तक उसका चक्र लगा ही रहता है। आवागमन बंद नहीं होता। तो जीव का परम लक्ष्य नित्यानंद ही है। दूसरे शब्दों में भगवान की प्राप्ति कहो, परमानंद आत्मा की प्राप्ति कहो। जी हाँ- मन जब तक भगवान आत्मा नित्यानंद का दर्शन नहीं पा लेता तब तक भटकता ही रहता है। उसका भटकना बंद नहीं होता। बस !
लोगों का कहना है कि जब मन स्थिर हो जाता है तब आत्मा का अनुभव होता है। तो फिर लक्ष्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन होने पर ही मन स्थिर होता है। आत्मदर्शन के बाद ही मन स्थिर होता है। क्या प्रमाण? सुनो हम इस पर लैला मजनूं का दृष्टांत कहते हैं। यह इश्क मिजाजी है और इश्क हकीकी का तो फिर कहना ही क्या है। इस कथानक में मजनूं का वास्तविक नाम कैश था, परन्तु लैला के प्रेम ने उसका नाम मजनूं कर दिया। यह इश्क मिजाजी की मिसाल है। उस मजनूं की दुनियाँ, सब कुछ लैला ही थी। जो इश्क मिजाजी में पागल हो तो उसे मजनूं कहते हैं और जो इश्क हकीकी में पागल हो उसे मफतूं कहते हैं। लैला एक बादशाह की लड़की थी। वस्तुतः लैला काली बदसूरत थी। संसार की निगाहों में भले ही लैला बदसूरत थी परन्तु मजनूं की निगाह में तो वह बदसूरत नहीं थी। राजा को मजनूं का लैला से प्रेम बर्दाश्त न हुआ और राजा ने मजनूं को जंगलमें कैद कर दिया। मजनूं के वियोग में लैला बीमार पड़ गई। इलाज के लिए हकीमों को बुलाया गया। हकीमों ने देखा कि कोई मर्ज हो तो दवा दी जाए परन्तु, राजा के डर से हकीमों ने सलाह दी कि लैला का खून खराब हो गया है। इसका खून निकालना होगा, तो नश्तर लगाकर खून निकाला गया, परन्तु कुछ लाभ न हुआ। कारण तो स्पष्ट ही था कि जब कोई बीमारी हो तो कुछ ठीक हो, अतः लैला को अच्छा करने के लिए जितनी भी दवाइयाँ की गई, सब बेकार हुई। लैला किसी भी हालत में अच्छी न हुई तो बादशाह और बेगम सोच में पड़ गए कि फिर क्या करना चाहिए। तो एक रात एकांत में लैला के विषय में चिंतित हो सलाह किए कि जब लैला और मजनूं का इतना प्रेम है तो विवाह कर दिया जाये, परन्तु शर्त यह है कि पहले मजनूं का पागलपन दूर हो जाये। सुबह दरबार लगा। जब बादशाह की महफिल जुड़ी तो बादशाह सलामत ने काजियों के समक्ष बेगम साहिबा की सलाह जाहिर की कि लैला और मजनूं की शादी की बात मानी जा सकती है, बशर्ते कि मजनूं का पागलपन दूर हो जाये। उसका पागलपन मिट जाने के बाद ही शादी की जा सकती है। काजियों ने इसकी ताईद की-जी हुजूरी हुई- मगर उस महफिल में एक सफेद दाढ़ीवाला बूढ़ा काजी उठकर खड़ा हुआ- जहाँपनाह । गुस्ताखी माफ हो-आपका फरमान है कि लैला से मजनूं की शादी हो बशर्ते कि मजनूं का पागलपन पहिले दूर हो जाये तो हुजूर ने यह भी कभी सोचा कि मजनूं आखिर पागल क्यों हुआ? बिना लैला के ही मजनूं पागल हुआ है। तो मजनूं का पागलपन बिना लैला के कैसे मिटेगा?
यही हालत मन की है यहाँ पर मानो कि लैला आत्मा भगवान है और मजनूं है मन। तो फिर मन किसकी तलाश में पागल की तरह भटक रहा है? परमानंद की फिराक में। उसे चाहिए सच्चिदानंद घनभूत, जिस स्वरूप का दर्शन जिसकी तलाश अनादिकाल से हो रही है। इस मन का जो पागलपन है, जो विक्षिप्त घूम रहा है, जुआड़ी, शराबी, दुराचारी, वैरागी, संन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी आदि बनता जा रहा है। मनीराम इनमें आनंद ढूँढ़ रहा है, आनंद को प्राप्त करने के लिए पागल हुआ घूम रहा है। तो समझ लो कि उसका यह पागलपन, उसका दोष नहीं है, व्यर्थ ही मनीराम पर आरोप लगाते हो। वह क्या करे पागलपन में रात-दिन भटक रहा है। एक स्त्री मर गई तो दूसरा किया आनंद के लिए, तीसरा, चौथा, घर में बाहर में भटक रहा है। चाहे वैरागी हो या दुराचारी हो-आनंद मिले, करके ही भटक रहे हैं, परन्तु मनीराम को नित्यानंद नहीं मिला है। और अभी तक अनादिकाल से घूम रहा है, उसी की तलाश में। जब तक नित्यानंद की प्राप्ति मन को न हो ले तब तक मन स्थिर न होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब इनकी अपील नहीं। दूसरे कोर्ट के फैसले की अपील तो होती है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखरी होता है। संतों का कोर्ट अध्यात्म विषयक सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ का फैसला सर्वमान्य होता है। इसको अब गीता द्वारा मंजित कर दें-
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः ।।
(गीता 2-16)
बुध तत्वदर्शियों की वाणी भगवान को भी मान्य होती है। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेना, यही मनीराम मजनूं के भटकने का कारण है। वह घूमेगा-जब तक 'मैं' का अनुभव न कर ले। ध्यान, धारणा, समाधि आदि मन का घूमना बंद करने के लिए करते हैं, परन्तु इन उपायों (ध्यान, धारणा, समाधि, जप, तप) से भी मन स्थिर नहीं होता। उसे तो आग लगी है लैला, भगवान की। वह भगवान चाहता है। आँख मूंदने से भगवान नहीं मिल जाते, मन को तो भगवान चाहिए, उसे नित्यानंद की भूख लगी है, उसे नित्यानंद मिले। जप, तप, ध्यान, धारणा, समाधि में नित्यानंद कहाँ? हाँ, ध्यान धारणा- समाधि (साधन) से मन कुछ देर के लिए रुक जाता है, उसकी प्रवृत्ति, चंचलता रुक जाती है और क्षणिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जप, तप में जब तक न समाहित है, आनंद मिला परन्तु जप से उठे नहीं कि आनंद चला गया इन सब विषयों में आनंद चाहे शुभ से हो या अशुभ से हो स्वरूप वही आनंद है, परन्तु यह आनंद क्षणिक है, अविनाशी, शाश्वत आनंद नहीं है। स्वरूप भगवान आत्मा को प्राप्त करना ही शाश्वत (नित्य) आनंद है और यह आनंद साधन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता।
हठ योग में योगी प्राण को ब्रह्माण्ड में चढ़ाकर ब्रह्मरंध में स्थापित कर लेता है। फिर संसार की तरफ उसका मन नहीं भागता, नहीं दौड़ता। परन्तु, जब योग से उपरत होता है, तो उसी समय, उपरत होते ही संसार सामने आकर खड़ा हो जाता है। मन चंचल हो उठता है। अरे यार! जगह-जगह नदी में तुम बांध भले डाल दो, परन्तु क्या नदी स्थिर हो जाती है? नदी का कार्य तो स्थिर नहीं होता वह निरंतर बांध को तोड़ डालने का प्रयास करती ही रहती है और कभी न कभी बांध को तोड़ डालने में समर्थ भी हो जाती है। बांध से नदी का प्रवाह बांध के मजबूत रहते तक रुका रहता है, परन्तु स्थिर नहीं होती। वह स्थिर तो समुद्र में जाकर मिलने से ही होती है। समुद्र में नदी को स्थिर करने के लिए बांध डालने की जरूरत नहीं है। अतः यह निर्विवाद है कि बांध डालने से नदी स्थिर नहीं होती, नदी तो समुद्र में ही पहुँचकर स्थिर होती है। यह तो सबको विदित ही है कि बांध टूट जाये तो सैकड़ों गाँव घर बह जाते हैं। बांध से कभी भी नदी का स्थिर होना सिद्ध नहीं है। मन रूपी नदी की कल्पना रूपी धार संकल्प-विकल्प रूपी किनारों पर निरंतर बह रही है और बिना साधन के डी (बांध के बिना ही) नित्यानंद सागर में ही लीन हो जाती है। जिस प्रकार बांध से चंद वर्ष, समय के लिए नदी की धार रुक जाती है, उसी प्रकार साधन ध्यान, धारणा इत्यादि) से कुछ समय के लिए मन रुक जाता है, परन्तु स्थिर हीं होता। नित्यानंद भगवान आत्मा को प्राप्त किए बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। हाँ-मन रूपी नदी की कल्पना रूपी धार को भले ही समाधि द्वारा रोक दो, परन्तु उससे उठे नहीं कि मन का व्यापार चालू हो जाता है। महर्षि पतञ्जल जी योग दर्शन में कहते हैं-
अभ्यास वैराग्याभ्याम् तन्निरोधः ।।
(योगदर्शन)
अभ्यास और वैराग्य द्वारा उसका (चित्त का) निरोध होता है।
योगश्चित्तवृत्ति निरोधः ।।
(योगदर्शन 1/2)
चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है।
योगश्चित्तवृत्ति निरोधः न तु चित्तवृत्ति स्थिरः ।।
जी, योग से मन की चंचलता का निरोध कहते हैं, न कि मन का स्थिा होना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इत्यादि साधनों से मन की चंचलता का निरोध भले ही हो जाये, परन्तु नित्यानंद भगवान आत्मा की प्राप्ति के बिना मन स्थिर न होगा। मन की भूख यही है। मन इसी को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए स्थिर नहीं होता और प्राप्त कर लेने पर स्थिर हो जाता है। बाह्य साधन (समाधि) से मन का निरोध होता है। अब यह प्रश्न होता है कि साधन से मन का निरोध ही होता है, स्थिर नहीं क्या यही बात है स्वामी जी? देखो समझ लो कि मन का निरोध करने के लिए ही साधन की आवश्यकता है, परन्तु मन को स्थिर करने के लिए कोई साधन नहीं। अरे! नदी को रोकना है तो साधन (बांध) की आवश्यकता है, न रोको तो वह स्वयं ही समुद्र में जाकर स्थिर हो जाएगी। भाई ! न रोकोगे तो नदी क्य आसमान में जाएगी? नदी का प्रवाह स्वभावतः समुद्र की ओर है, चाहे रोक तब और न रोको तब, वह समुद्र में ही जाएगी और कहाँ जाएगी? बांध सिर्फ रोकने मात्र का साधन है। परन्तु नदी के वेग को स्थिर करने के लिए कोई साधन नहीं है। इसी तरह मन की चंचलता को रोकने का साधन समाधि है समाधि द्वारा रोकी जा सकती है, परन्तु स्थिर कहाँ होगी? नित्यानंद में और नित्यानंद को प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है। नित्यानंद कृपा साध्य है। मन को नित्यानंद का दर्शन कराना चाहो तो संत कृपा प्राप्ति के लिए साधन करो, उसकी शरण में जाओ। आत्म दर्शन की प्राप्ति सद्गुरु ही कराएंगे। इसलिए उन्हीं की शरण में जाना होगा। साधनों की कमी नहीं है, परन्तु इससे मन को शांति, मन को विश्राम नहीं मिलना है। आपको इस तरह से प्रमाणों द्वारा एवं संत वाक्यों द्वारा समझाया गया कि मन की स्थिरता चाहते हो तो संत कृपाभिलाषी बनो। यह कृपासाध्य वस्तु है। जी हाँ यह भली भाँति समझ लो कि नित्यानंद ही मन को चाहिए। आत्मसुख प्राप्त करने के लिए ही मन व्यग्र है। श्री मानसकार भी यही कहते हैं-
निज सुख बिनु मन होई कि थीरा। परस कि होई विहीन समीरा ।।
अब तो मिल गया प्रमाण। 'निज सुख बिनु मन होई कि थीरा' आत्म सुख, ब्रह्म सुख, निजानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद मन को चाहिए।
निज सुख बिनु मन होई कि थीरा । परस कि होई विहीन समीरा ।।
जब तक आत्म सुख, निजानंद न प्राप्त कर ले तब तक मन स्थिर नहीं होता। 'शिव' लाख साधन करो, कुछ भी करो, मनीराम का पागलपन तो देखो-कभी कोई वेश बनाता है, कहीं जाता है, कहीं पहाड़ों पर भटकता है- जितना स्वांग करता है, जो कुछ भी करता है, मन का ही प्रताप है। जिस दिन आत्म-दर्शन कर लेगा उसी दिन आत्म सुख अनुभव करते ही मंजिल खतम हो जाएगी। फिर चलना कहाँ? मंजिल तो घर (मुकाम) पर पहुँचते ही खतम हो जाएगी। अपना घर टूटा-फूटा ही क्यों न हो भैया ! सुख की नींद तो वहीं आती है। क्यों नहीं? पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं, परन्तु विश्राम अपने घोंसले में ही पाते हैं। जब तक अपने घोंसले में नहीं आ जाते तब तक विश्राम कहाँ? मन रूपी पक्षी इस विस्तृत विषयाकाश मंडल में अनादिकाल से उड़ रहा है। संकल्प-विकल्प उसके दोनों पंख हैं। संसार के विषयों में आदिकाल से उड़ रहा है और जब तक अपने स्वरूप आत्मा रूपी घोंसले में नहीं आ जाता, उसका उड़ना बंद नहीं होता-तब तक मन को शांति नहीं मिलती।
यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यदजितेन्द्रियः ।।
(7 - 4 - 19)
अजितेन्द्रियः हिरण्यकशिपुः नातृप्यत् । हिरण्यकश्यप का मन तृप्त न हुआ। इतने ऐश्वर्य भोगों की उपलब्धि से भी वह संतुष्ट न हुआ। उसका मन शांत न हुआ। उसका वैभव तो उसके तपोबल के प्रभाव से प्राप्त हुआ था। हाँ-वह तपोबल है। तप के प्रभाव से उसे इस तरह अणिमादिक सिद्धियाँ प्राप्त हो गई थीं। यह सब तप का प्रभाव है, फल है। व्याकरण में तप-ऐश्वर्य धातु है। तप का फल ही है ऐश्वर्य की प्राप्ति। वह नित्यानंद का फल नहीं था। जो हिरण्यकश्यप ने प्राप्त किया।
मजा आ गया-नातृप्यदजितेन्द्रियः । हृदय का पता तो लगे कि हम चाहते क्या हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? और यह भी देखो जब पानी की एक बूंद देखते हो तो अनुमान होता है कि कहीं न कहीं इसका सागर है। सांसारिक विषयों के मिल जाने से जो आनंद मिलता है वह कहाँ का कतरा है? वह कहाँ की बूंद है? कहीं न कहीं इसका सागर होगा ही। जब क्षणिक आनंद में मन इतना विभोर हो जाता है तो फिर उसका (नित्यानंद का) क्या कहना है, वर्णन नहीं हो सकता। वह आनंद मन, वाणी का विषय नहीं है।
ब्रह्म पियूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावै ।
तौ कत मृगजल रूप विषय कारण निशिबासर धावै ।।
(विनय 116)
जैसे मृग, मृगजल (मृग तृष्णा के जल) की ओर क्यों दौड़ रहा है? वह कब तक दौड़ेगा। जब तक उसे वास्तविक जल नहीं मिल जाएगा तभी तक वह दौड़ेगा। इसी तरह मन रूपी मृग विषयानंद रूपी मृग तृष्णा के जल की ओर तभी तक दौड़ता है जब तक उसे ब्रह्मानंद रूपी वास्तविक जल की प्राप्ति नहीं हो जाती।
माधव ! असि तुम्हारि यह माया ।
करि उपाय, पचि मरिय, तरिय नहिं, जब लगि करहु न दाया ।।1।।
सुनिय, गुनिय, समुझिय, समुझाइय, दशा हृदय नहीं आवै ।
जेहि अनुभव बिनु मोहजनित, भव दारुन विपति सतावै ।।2।।
ब्रह्म पियूष मधुर शीतल, जो पै मन सो रस पावै ।
तौ कत मृग जल रूप विषय, कारण निशिवासर धावै ।।३।।
जेहि के भवन विमल चिंतामणि, सो कत काँच बटौरै ।
सपने बरबस परै जागि, देखत केहि जाइ निहोरै ।।4।।
ग्यान, भगति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही ।
तुलसीदास हरि कृपा मिटै भ्रम, यह भरोस मन माहीं ।।5।।
हाँ जी-
देवता तो हिरण्यकश्यप के देवलोक पहुँचने के पहले ही भाग खड़े हुए थे. पर्वत की कन्दराओं में जा छिपे थे। देवताओं ने भगवान के पास जाकर प्रार्थना की, अपने महत् कष्टों का वर्णन किया और साष्टांग नत हो प्रार्थना की कि भगवन् ! कृपा हो-त्राहि माम् त्राहि माम्। रक्षा करो, रक्षा करो इस हिरण्यकश्यप से। तो भगवान नारायण द्वारा उनका दुःख देखकर मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी हुई।
मा भैष्ट विबुध श्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः ।
मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ।।
ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च ।
तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत्प्रतीक्षत् ।।
यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु ।
धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति ।।
निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने ।
प्रह्लादाय यदा द्रुह्येद्धनिष्येऽपि विरोर्जितम् ।।
( श्रीमद् भागवत 7-4-25, 26, 27, 28)
देवता, देव, गौ, ब्राह्मण, साधु, धर्म तथा मुझसे द्रोह करने वालों का नाश शीघ्र ही हो जाता है। हिरण्यकश्यप के प्रह्लाद नाम का पुत्र होगा वह महा भागवत (ब्रह्म पारायण) होगा। जब हिरण्यकश्यप उससे द्वेष करेगा तब उसका नाश हो जाएगा। तुम लोग समय की प्रतीक्षा करो। देवता लोग इस गंभीर आकाशवाणी को सुनकर संतुष्ट हो, अभय होकर लौट गए।
कालांतर में हिरण्यकश्यप के चार पुत्र हुए- आह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और प्रह्लाद। प्रह्लाद सबसे छोटे थे और गुणों में सबसे बड़े। वे संत, देवी, गौ, ब्राह्मण के सेवक, भक्त सौम्य स्वभाव, सत्य प्रकृति एवं जितेन्द्रिय थे। उनकी दिनचर्या भगवद्भक्ति थी। भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाते थे।
आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रियसुहृत्तमः ।।
(श्रीमद् भागवत 7-4-31)
वे समदर्शी थे, सदैव हरिः शरणं, हरिः शरणं की ध्वनि उसके मुखारविन्द से निरंतर निकलती रहती थी। जब प्रह्लाद पाँच वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने अपने दैत्य कुल के आचार्य शण्डामर्क को बुलाकर प्रह्लाद की शिक्षा का भार दिया। उन्हें सचेत कर दिया कि प्रह्लाद को दैत्यकुल की परम्परानुसार अच्छी शिक्षा दी जाये? प्रह्लाद 4-6 माह पाठशाला नित्य जाते रहे। एक दिन उसकी माता कयाधू ने इसे स्नान कराकर, सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके, पिता हिरण्यकश्यप के पास नमस्कार करने को भेजा। प्रह्लाद ने अपने पिताजी को तनिक दूर खड़ा होकर नमस्कार किया तो हिरण्यकश्यप ने प्रेम से गोद में बिठाकर पूछा-बेटा !
पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान् ।।
(7 - 5 - 4)
तुम्हें स्कूल जाते बहुत दिन हो गए, बताओ कि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया? बताओ तुम्हें कौन-सी बात अच्छी लगती है। प्रह्लाद कहता है- पिताजी ! सुनिये-
तत्साधुमन्येऽसुखर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् ।
हित्वाऽऽत्मपातं गृहमंधकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ।।
(7-5-5)
हे असुरवर्य (दैत्यों में श्रेष्ठ) पिताजी ! यह मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलताहै, परन्तु इस गृहस्थाश्रम में कुछ न कुछ विक्षेप होता ही रहता है, चित्त एकरस नहीं रहता। हमेशा कोई न कोई अशांति मन में बनी ही रहती है। चाहे वह पुत्र से हो, भाई से हो, कुटुम्बियों से हो, पड़ोसियों से हो, कोई न कोई उद्विग्नता चित्त में हमेशा बनी ही रहती है। यह गृहस्थाश्रम आत्मपात और अन्धकूप है। इस आश्रम में क्षण, प्रतिक्षण आत्मा का पतन होता रहता है। अब विचार करना है कि इस आश्रम को प्रह्लाद ने आत्मपात क्यों कहा? आत्मा के पतन का क्या स्वरूप है? शुद्ध तत्व भगवान आत्मा को कुछ न कुछ मान लेना ही आत्मा का पतन है और गृहस्थाश्रम में रहने से कुछ न कुछ माना ही पड़ता है। बस, फिर गोविन्दाय नमो नमः-
शुद्ध तत्व भगवान आत्मा में अपनी मान्यता आरोपित करते हैं कि मैं पति हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, भाई हूँ आदि। कुछ न कुछ अपने 'मैं' को मानता ही रहता है और जहाँ अपने आपको कुछ भी माना तो यही आत्मा का पतन है, सूत्र लिखो- 'मान्यता का पर्याय प्रपंच है।' गुफा में बैठना प्रपंच का त्याग नहीं है। 'मैं' जैसा हूँ वैसा न जानकर कुछ न कुछ मान लेना ही आत्मा का पतन है। इसीलिए यह आश्रम आत्मपात है। चाहे वह क्षणभर के लिए ही क्यों न हो प्रपंच (मान्यता जगत) में आना ही आत्मा का पतन है। फिर देखो-महात्मा प्रह्लाद कहते हैं कि गृहस्थाश्रम अंधकूप है-अंधकूप किसको कहते हैं? क्या भाव है? देखो-कहीं पर बड़ा भारी कुआँ है। उसके चारों ओर लम्बी-लम्बी धास उग आई है और इन तृण लताओं करके कुआँ पूर्णतया ढँका है। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब कोई पशु उधर से चरने को निकला। लम्बी- लम्बी हरी-हरी सुंदर घास देखकर चरते-चरते ज्यों ही वह आगे पैर बढ़ाता है तो नीचे कुएँ में गिर पड़ता है। गिरा तो निकलना मुश्किल है। जी हाँ-अब इसका भाव क्या है? यह जो गृहस्थाश्रम है वह अन्धकूप है। सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, सुंदर मकान, आज्ञाकारी नौकर, भोग की सारी सामग्री, यह मानो हरी- हरी घास है। इस तृणलता करके गृहस्थाश्रम रूपी कुआँ ढँका हुआ है। अब गृहस्थ पशु किसको कहै? अरे ! वही जो मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्री हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यासी हूँ, बालक, युवा, वृद्ध हूँ, लम्बा हूँ, चौड़ा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, ऊँचा हूँ, नीचा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ आदि मानता है। 'ईदृशी धारणा येषाम् ते सर्वे पशवः।' ऐसी जिनकी धारणा है वे सब बिना सींग पूछ के पशु हैं। अच्छा फिर देखो त्रिगुणात्मक मान्यताओं से परे 'मैं' आत्मा हूँ। अरे भाई ! इनका साहित्य अलग-अलग होता है। तुमने ही माना कि शरीर हूँ तो फिर शरीर के धर्म-मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, मैं शाक्त हूँ, बौद्ध हूँ, जैन हूँ इत्यादि, वर्णी हूँ, आश्रमी हूँ, ये शरीर के धर्मों की मान्यता हो जाती है। जहाँ मैं शरीर हूँ, ऐसा माना तो फिर 'मैं' में मैं शरीर और मेरा शरीर, यह धर्म सब आ गए। अच्छा-अब तुम्हारे ऊपर मिसपरसॉनिफिकेशन (गलत हुलिया) बताने का जुर्म क्यों न लगाया जाए? ताजरात हिन्द जाप्ता फौजदारी की दफा क्यों न कायम की जाये? 'मैं' जैसा हूँ वैसा न बताकर अपने आपको साढ़े तीन हाथ का शरीर बतना दफा 468 का जुर्म है। जाओ-वकीलों से पूछ लो और इसकी सजा है जन्म और मरण। बोलो 'मैं' जैसा हूँ वैसा न बताकर, 'मैं' संसारी जीव हूँ, बताना, अपने आपको जीव मानना यह जुर्म नहीं तो और क्या है? जाओ, फिर इसकी सजा भुगतो-चौरासी लाख योनियों में भटको। यही तुम्हारी इस मान्यता की सजा है। जीव मानने की सजा भुगतनी ही होगी। अपने आपको शुद्ध तत्व आत्मा न जानकर संसारी जीव मानने की यही सजा है आवागमन। मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पुण्यी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, इन सब मान्यताओं का चार्ज तुम पर लग गया। हाँ-बिल्कुल और भोगो इनकी सजा-
अरे! यह जो मान्यता है कि मैं ब्रह्म हूँ, यह भी गलत हुलिया बताना है। राम राम ! सीता राम !!
जैसा 'मैं' हूँ वैसा ही हूँ। परन्तु, पहले अपने 'मैं' में 'मैं' ब्रह्म हूँ, यह आरोपित कर रहे हो, बड़े बन रहे हो। अकड़कर कहते हो कि मैं त्यागी हूँ, मैं द्रष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, यह ब्रह्मभाव सतोगुणी मान्यता है। अपने को ब्रह्मज्ञानी मानते हो तो किसकी अपेक्षा से? दूसरों को अज्ञानी मानकर ही तो अपने को ज्ञानी बताते हो? अतः इसकी सजा है-ज्ञान का प्रमाद? तुम्हारी दृष्टि में जीव दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारा यह ब्रह्मभाव जीव की अपेक्षा से ही तो है कि ब्रह्म की अपेक्षा से ब्रह्मभाव है? बोध तो उसको कहते हैं कि 'मैं' के सिवाय अन्य कुछ नहीं, और कुछ न दिखै। जब मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव रखते हो तो जीवभाव इसका विरोध करता है। जीववादी विरोध करेगा। बड़ी मुश्किल है। जहाँ देखो वहाँ राग-द्वेष। क्या 'मैं' का भी कोई विरोधी है? 'मैं' इस आत्म तत्व में सब विरोध समाप्त हो जाते हैं, 'मैं' का 'मैं' शुद्ध तत्व का बोध हो जाता है। इसलिए यह गृहस्थाश्रम अन्धकूप है। देहासक्त, दारासक्त, पुत्रासक्त यही देहाभिमानी पशु है। फिर इसको ध्यान से देखो-क्या सभी गृहस्थाश्रम अन्धकूप है? क्या सभी गृहस्थ अन्धकूप में हैं। नहीं, जो देहाभिमानी हैं, अपने आपको कुछ माने हुए हैं, वे ही अंधकूप में हैं। वैसे तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बड़े-बड़े महात्मा, ऋषिगण, वशिष्ठ, अत्रि, गोते तो अगस्त्य सभी गृहस्थाश्रम में हैं। भगवान कृष्ण तो राम-राम महागृहस्थ हैं- सोलह हजार एक सौ आठ तो प्रमाणित पत्नियाँ हैं और बाकी भगवान ही जानें। अगर इनमें गृहस्थाश्रम का दोष मानोगे तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। ये भी पशु कहे जाने लगेंगे। अरे ! पशु तो देहाभिमानियों के लिए कहा गया है। अज्ञानी गृहस्थों के लिए पशु संज्ञा दी गई है, न कि बोधवान गृहस्थ के लिए। यह प्रह्लादोपाख्यान बड़ा ही सुंदर है। जी हाँ-ध्यान से सुनो, अब चीज यहाँ-
तत्साधुमन्येऽसुर वर्यं देहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् ।
हित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ।।
(भाग. 7-5-5)
इसका इसलिए परिहार किया जाता है। सीता स्वयंवर के लीला भाग में जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की रचना कर रहे थे, तो उसी प्रसंग में लिखे कि-
शंकरचाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल ।
बूड़े सकल समाज.... ।।
यहाँ तक तो लिख गये-फिर विचार किया कि यह क्या अनर्थ कर डाला, सीता स्वयंवर में, उस समाज में तो संत महात्मा भी बैठे थे। स्वयं श्री जनक जी महाराज, श्री विश्वामित्र जी और अन्यान्य ऋषिगण बैठे थे। तो फिर क्या वे भी डूब गये? नहीं, मुझसे बड़ी गलती हो गई। रामायण में हर ताल तो लगाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो-
शंकरचाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल ।
बूड़े सकल समाज... ।
तीन ही चरण लिखे थे। यह पद उस समय का है जब सहस्त्रों राजा महाराजा प्रयत्न करने पर भी शंकर जी का धनुष न उठा सके। अरे ! थोड़ा भी न हटा सके तो जनक जी महाराज बड़े परिताप में डूब गए।
तजहु आस निज गृह जाहू। लिखा न विधि वैदेहि विवाहू ।।
आदि! उन्हें बड़ी निराशा हुई। वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान शंकर का धनुष (चाप) मानो जहाज के समान था और श्रीराम का बाहुबल ही मानो समुद्र था। तो पिनाक रूपी जहाज में सभी समाज बैठा था। अब 'सागर' रघुबर बाहुबल के ऊपर फिर लिखते हैं कि 'बूड़े सकल समाज', तो समाज में तो सभी बैठे थे। बड़े-बड़े संत महात्मा भी उस समाज में ही थे। तो क्या वे भी डूब गये? उनका सिर चक्कर खा गया। विचार करते-करते सिर घूम गया। तो उठ बैठे और चले गए गंगाजी स्नान आदि करने के लिए। तीन चरण तो लिख गये थे चौथा चरण लिखना बाकी था। तो श्री हनुमान जी उसे पूरा कर दिये कि चढ़े जो प्रथमहिं मोहबस ।। यानी शंकरचाप जहाज से वे ही डूबे जो मोहवरा चढ़े थे। अरे! अज्ञानता के कारण जो अहंभाव लेकर गये थे कि हम ही सीता से विवाह करेंगे, वे डूबे। अतः गलती न हो जाय इसलिए परिहार करते हैं- ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, राम, कृष्णादिक ये सब गृहस्थ हैं। तो फिर सभी गृहस्थों को पशु नहीं कह सकते। जो देह को ही आत्मा माने हुए हैं, ऐसे देहाभिमानी ही अंधकूप में गिर रहे हैं और वे ही पशु हैं, न कि सब।
तत्साधुमन्येऽसुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियामसङ्ग्रहात् ।
हित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ।।
(भा. 7-5-5)
उपदेश तो ऐसे सब जीववादी गृहस्थों के लिए कर रहे हैं और (दबी जबान में) कहते हैं कि ये भी गृहस्थ हैं-संन्यासी दिखने मात्र के जो हैं। उपदेश गृहस्थों का हो रहा है। इने-गिने संन्यासी वस्तुतः है जो कि नहीं के बराबर। इने-गिने इसलिए, क्योंकि संन्यासी का कोई बाजार नहीं है। संन्यासी का भाव क्या है? क्या अर्थ है?
ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ।।
(गीता 5/3)
उसे ही नित्य संन्यासी जानो कि जो राग-द्वेष नहीं करता। ऐसा ही निर्द्वन्द्र है, वह सुख रूपी बंधन से भी छूट जाता है। जिसका मोह सम्यक् प्रनिर्दिन्य नष्ट हो गया है-यही संन्यासी का अर्थ होता है। सिर्फ काशाय वस्त्र धारण कर लेना, शिखा, सूत्र का परित्याग कर देना ही संन्यासी का लक्षण नहीं है। काषाय वस्त्रधारी शिखा, सूत्रहीन को संन्यासी मान लेना वस्तुतः ठीक नहीं है। इसलिए संन्यासी कम हैं। सम्यक् प्रकार से समझने वाले भी कम हैं। भैया! जी हाँ- शिव शिव हाँ जी-
तत्साधुमन्येऽसुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियामसङ्ग्रहात् ।
हित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ।।
(भा. 7-5-5)
इस वैराग्य युक्त वाणी को सुनकर कुछ लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि यदि स्वामी जी पहले मिले होते तो इस गृहस्थाश्रम के चक्कर में न पड़ते। तो भैया ! अब क्या बिगड़ा है? कहते हैं कृपा करो-बड़े चक्कर में पड़े हैं। अगर आप पहले मिले होते तो-खैर, अब क्या बिगड़ा है? जिंदगी भर क्या गृहस्थी में ही रहने का ठेका सिर पर ले रखे हो? अगर हिम्मत हो तो चलो हमारे साथ तुम भी। अरे, हाँ भाई ! ब्रज की एक बोली है-'राँड़ के पाँव सुहागिन लागै हो जा बहिना मोसी।' जब कोई सुहागिन स्त्रिी किसी विधवा स्त्री का पैर पकड़ती है तो भीतर ही भीतर, मन ही मन वह कहती है कि तू भी मेरे समान हो जा। बाहर कहे तो सिर न फोड़ दे। वह मन ही मन कहती है- जैसे मैं हो गई हूँ, वैसे ही तू भी हो जा। हम भी यही आशीर्वाद देते हैं कि भैया ! हमारे समान तुम भी हो जाओ। बहुत दिन हो गए गृहस्थी का मजा लेते, अब जरा फकीरी का भी मजा लो। परन्तु बात-जैसे चोकर अटक गया हो, बाहर आये न भीतर जाय। चोकर का मतलब (अब स्वामी जी चोकर का मतलब बताते हैं) दिल्ली शहर में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी रहते हैं। गेहूँ का आटा छान लेने के बाद चलनी में जो बचा रहता है उसे चोकर कहते हैं। गरीब बच्चों की मातायें बाजार से चोकर ले आती हैं और उसको साफ कर लेती हैं। चोकर को पंजाब में बूर भी कहते हैं, जरा घी में उसको भून लेती हैं और थोड़ा गुड़ का शीरा जो कि हुक्का के गुड़ाखू बनाने के काम में आता है, चोकर मिलाकर उससे सुंदर छोटे-छोटे लड्डू बना लेती हैं। फि शाम के समय उन लड्डूओं को छोटी-छोटी सुंदर टोकरियों में सजा देती है ऊपर से खस, केवड़े आदि का इत्र छिड़क देती हैं। सुंदर गजरा, फूल कायस रखकर गरीब बालक अब उसे बेचने के लिए शहर के पार्कों में जाते हैं। रिस में चिकना चुपड़ा तेल लगाकर बुश शर्ट पहिने, बड़े लहजे के साथ ये लड़के दुपल्ली टोपी लगाकर नजाकत के साथ बेचने निकलते हैं। बाहर से आये सैलानी पार्क में बैठे रहते हैं। किला ग्राउण्ड और अन्य पार्कों में जहाँ देखते हैं कि ये सैलानी बाहर के हैं, एक बेंच में 4-6 बैठे पार्क का मजा लेते देखते हैं तो लहजे से उनके पास पहुँचते हैं-बाहरी देख लेते हैं क्योंकि, जानते हैं कि वहाँ के रहने वालों से सौदा नहीं होगा। अब कहते हैं-ले ले दिल्ली के लड्डू आने में एक, जो खाये वह पछताये, न खाये वह भी पछताये। कहते तो सच्ची बात हैं। परन्तु लहजे से कहते हैं। बाहर के सैलानी बालक को पैसा देकर सब लड्डू खरीद लेते हैं और एक-एक लड्डू बांटकर जब गप लगाते हैं तो चोकर तो चोकर, मिठास तो अंदर चला जाता है, परन्तु चोकर भीतर नहीं जाता। नाक, आँख, सब भर जाता है, लाल-लाल मुँह हो जाता है, स्वाँस लेना बंद हो जाता है। नाहक पैसा फेंका दूसरी बात। तो भैया! यही दिल्ली का लड्डू है। वैराग्य का उपदेश सुनकर मन में परिवर्तन होता है कि स्वामीजी गृहस्थी बिना छोड़े मजा कहाँ मिलेगा? परन्तु, यही चोकर वाली बात-चोकर का त्याग नहीं कर सकते। गृहस्थाश्रम छोड़ के भाग जाओ कहें तो कहते हो पाप लगेगा। यह भी विकल्प ही है। स्त्री, बाल-बच्चों को छोड़कर कैसे भागें? उनको कष्ट होगा तो पाप लगेगा। जब स्त्री का बच्चा पेट में रहता है तो तुम खिलाने गए थे, तुम गए थे पालन करने? जो परमात्मा विश्वम्भर है क्या उस पर तुम्हारा भरोसा नहीं है, जो भगवान बच्चे के पैदा होने के साथ ही माँ के स्तन में दूध पैदा कर देता है? अब यदि भैया! रहते हो तो यह तुम्हारी ही कमजोरी है, क्योंकि चोकर जो अटक गया है।
जी हाँ-जब टट्टी लगती है तो पैदल भागते हो-तब किसी की सुनते भी नहीं, लोटा लेकर भागते हो, फिर कुछ नहीं सूझता। उस समय लज्जा, भय कुछ नहीं रहता। इसी तरह मनीराम को प्रपंच रूपी मल त्याग करने की जब हाजत होती है उस समय फिर न स्त्री, न बाल - बच्चे, न घर-बार कुछ भी नहीं दिखाई देता। पास में स्त्री सोई हुई है, उठा और चल देता है। तो फिर जुलाब दिया जाता है कि टट्टी लगी-फिर साधु बने। इसे जुलाब लेने की जरूरत है। मनीराम को तो साधु ही जुलाब देंगे। संत की वाणी ही जुलाब है।
तत्साधुमन्येऽसुखर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् ।
हित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ।।
महात्मा प्रह्लाद कहते हैं-पिताजी ! इस गृहस्थाश्रम को छोड़ देना और वन में जाकर श्री हरि आत्मदेव की शरण में हो जाना, यही शिक्षा मैंने पाठशाला में अपने गुरुजी से ली है।
श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः ।
जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः ।।
(श्रीमद् भागवत 7-5-6)
हिरण्यकश्यप हँस पड़ा-अरे भाई! अभी यह बच्चा है। 5 साल का ही है। तोता-मैना को जैसा सिखा दो वैसा ही वे बोलते हैं। इसी प्रकार बालक तोता- मैना के समान ही होते हैं जैसा कुछ वे सुनते हैं वैसा ही रट लेते हैं। उन्होंने प्रह्लाद के आचार्य को बुलाकर सावधान किया कि इसकी शिक्षा ठीक दैत्य कुल के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसा उपाय करो कि यह सुधर जाये। एकांत में गुरुजी को बता दिया कि सावधान रहना, प्रह्लाद का मनोभाव स्पष्टतया बिगड़ चुका है। उसकी बुद्धि बिगड़ गई है। ले जाओ, इसे ठीक से पढ़ाओ। जान पड़ता है कि आपके घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण छिपे पड़े हैं। अब वे इसको बहकाने न पायें। जब प्रह्लाद गुरुजी के यहाँ गए तो गुरुजी पुचकार कर पूछते हैं-
वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मा मृषा ।
बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः ।।
(श्रीमद् भागवत 7-5-9)
बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत् ।
भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन ।।
(श्रीमद् भागवत 7-5-10)
बेटा प्रह्लाद ! अभी तुमने अपने पिताजी से जो कहा और तुम्हारे पिताजी ने शिकायत की कि तुम किसी बहकाने में आ गए हो-तो क्या बात है? क्या सचमुच में तुम किसी के बहकावे में आ गए हो? तुमने अपने पिताजी से कहा कि अंधकूप एवं आत्मा का पतन करने वाले गृहस्थाश्रम को छोड़कर वन में चले जाना और श्रीहरि भगवान आत्मा की शरण में हो जाना चाहिये, इत्यादि ये सब अंड-बंड तुम क्या बक रहे थे? यह सब बदनामी की बात है। दैत्यकुल की परम्परा के विरुद्ध है। अतः ठीक-ठीक हमसे बताओ - 'मा मृषा', झूठ २ बोलना, तेरी बुद्धि को किसने हेरफेर कर दिया? तेरी बुद्धि को कौन बिगाड़ रहा है? तो प्रह्लाद कहता है-सुनिये गुरुदेव !
स्व परश्चेत्यसद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः ।
विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः ।।
(श्रीमद् भागवत 7-5-11)
क्या विलक्षण भाव है-गुरुजी सुनिये यह मेरा है, यह तेरा है, मैं-मैं हूँ तू-तू है, तू भिन्न है, मैं और हूँ, तू और है, इस प्रकार का भ्रम असत्य भावना, विपरीत भाव, पशु बुद्धि जिसकी माया करके अर्थात् जिसके अज्ञान से हो जाती है।
स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते ।
अन्य एष तथान्योऽहमिति भेदगता सती ।।
(श्रीमद् भागवत 7-5-12)
जिसके अज्ञान से असत्यभाव बुद्धि में बैठ जाता है, ऐसी पशु बुद्धि हो जाती है और जब उसका ही ज्ञान (बोध) हो जाता है तो इस पशु बुद्धि का नाश हो जाता है। तब वह कौन? क्या है? इस प्रकार के अज्ञान का लोप हो जाता है. तो फिर वह कौन है?
स एष आत्मा स्वपरेत्यबुद्धिभिर्दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते ।
मुह्यन्ति यद्वत्र्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्यादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम् ।।
शिव शिव-वह कौन है? स-भगवान आत्मा, अर्थात् जिसके अज्ञान से पशु बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसी को जानना चाहिए कि वह कौन है? अरे ! अपना आप आत्मा ही है। अपने आप आत्मा के ही अज्ञान से पशु बुद्धि हो जाती है। देखो-आत्मा किसको कहते हैं? उसका क्या लक्षण है? जिसके बिना जो एक क्षण भी न रह सके वहीं उसकी आत्मा है। डंडा लकड़ी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता इसलिए लकड़ी हुई डंडे की आत्मा। लकड़ी न हो तो डंडा अपना अस्तित्व किसमें रखेगा? इस तरह डंडे की आत्मा हुई लकड़ी। इसी तरह आभूषण की आत्मा सोना, कपड़े की आत्मा धागा, घड़े की आत्मा मिट्टी। आत्मा कहते हैं अस्तित्व को। जहाँ देश, काल, वस्तु नहीं-उसको आत्मा कहते हैं। जो जिसका आधार होता है वही उसका स्वरूप होता है। तो डंडे का स्वरूप लकड़ी है। जो जिसका स्वरूप होता है। वही उसका कारण होता है जो जिसका कारण होता है वही उसमें व्यापक होता है। जिस समय यह बोध हो जाता है, जब यह अनुभव कर लेता है उस समय उपरोक्त पशुबुद्धि का नाश हो जाता है, इसलिए अपना आप मैं आत्मा हूँ, इस बोध को प्राप्त करना चाहिए। संसार में बड़े-बड़े विद्वान, शास्त्रज्ञ, षट् शास्त्री हैं, बड़े- बड़े दर्शनाचार्य हैं, दर्शनशास्त्र के परिज्ञाता हैं, परन्तु उन्हें आत्मतत्व का बोध (अनुभव) नहीं है। वे ही विद्वान कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा भिन्न- भिन्न हैं।
दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते ।।
संसारी विद्वान क्यों न भिन्न-भिन्न मानें क्योंकि बड़े-बड़े वेदवादी ब्रह्मादिक भी आत्मा का निर्णय करने में मोहित हो जाते हैं। अतः प्राकृत संसारी विद्वानों का आत्मा को न जानना अथवा आत्मा परमात्मा में भेद मानना कोई आश्चर्य नहीं है।
मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ब्रह्येष भिनत्ति मे मतिम ।।
तो संसारी विद्वानों की बात ही क्या है।
अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि भगवान आत्मा को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान पाते, जानने में समर्थ नहीं हैं, तो कैसे समर्थ नहीं हैं? हाँ जी, नहीं है। शिव-देखो-यदि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भगवान आत्मा से भिन्न हैं तो वे हैं ही नहीं और अभिन्न हैं तो जानेंगे किसको? यदि भिन्न होंगे तो आत्मा नहीं अनात्मा होंगे। अरे भाई ! देखो वेदवादी ब्रह्मा आत्मा से यदि वस्तुतः भिन्न हैं तो यह अनात्मा हुआ और अनात्मा वस्तु जड़ होती है। तो अनात्मा आत्मा को क्या जानेगा और यदि अभिन्न है तो जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अनात्मा आत्मा को क्या जानेगा और यदि अभिन्न है तो जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह नई चीज है। यदि तुम अपने आपको भगवान से भिन्न मानते हो तो तुम हो गये अनात्मा और इस दशा में भगवान आत्मा को कैसे जानोगे? देखो ध्यान से समझना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि मैं कब मानना कह रहा हूँ और कब जानना। मानना और जानना में रात-दिन का अंतर है।
भगवान से अपने आपको भिन्न मानते हो तो भिन्नता मानने में है और अभिन्नता जानने में है। भिन्न करके मानते हो तो जड़ हुए इसलिए तुमको भगवान आत्मा को जानने में अधिकार ही क्या है और यदि अभिन्न जानते हो तो जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी भगवान आत्मा को जानेगा तो भगवान होकर ही जानेगा। भगवान होकर ही जाना जाता है। नदी समुद्र होकर ही समुद्र को जानती है, न कि नदी रहकर। नदी का समुद्र को जानना समुद्र होकर ही होगा, नदी रूप से नहीं। 'देवो भूत्वा देवं यजेत्।' जिसका पूजन करना है वह तुम स्वयं हो जाओ। देखो जब तुम किसी कांग्रेसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हो तो क्या भेंट करने के लिए जो पहिने हो उसी को पहनकर जाओगे? घर में भले ही मिल का कपड़ा, पहने रहो, परन्तु जब मिलना होगा तब जवाहर जाकेट, हाथ में रिस्ट वॉच बांधे, पैर में चप्पल और सिर पर श्री नॉट थ्री की टोपी, इस वेश में मिलोगे। हाँ भाई ! निशाना अचूक होना चाहिए। यही पोश बनाकर तो नेताजी से मिलोगे? जी हाँ-जो जैसा होता है, उससे वैसा ही बनकर मिलना होता है। जुआड़ी से दोस्ती करना है तो जुआड़ी बनकर ही दोस्ती होगी। परशियन में मियां शेखशादी का एक शेर है-
कुनद हम जिन्स हम जिन्स परबाज ।
कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज ।।
जो कुछ भी करना है तो वही होकर करना होगा। सजातीय सजातीय से प्रेम होता है न कि सजातीय विजातीय से। हाँ-सजातीय सजातीय से प्रेम होता है। तुम वही हो जाओ-इसीलिए हजरत ईसा ने किसी वक्त कहा है-कम यू नैकेड टू दी नैकेट क्राइस्ट। नंगे ईसा के पास नंगे होकर आओ क्योंकि ईसा नंगा है। ईसा से मिलना है तो तुम भी नंगे हो जाओ। ईसा नंगा है अर्थात् ईसा मान्यता रहित है। मैं अमूक हैं-इस अमुक रूपी विकल्प से ईसा रहित है। मुझ आत्मा को जानना हो तो मान्यता से परे हो जाओ। यह अटल निर्विवाद सिद्धांत है। यदि ब्रह्मादिक भी कहे कि मैं अमूक (ब्रह्मा हूँ) तो वह भी भगवान को जानने में समर्थ नहीं है।
स एष आत्मा स्वपरेत्यबुद्धिभिर्दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते ।
मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो होष। भिनत्ति मे मतिम् ।।
स एष भगवान आत्मा मे मतिम् (बुद्धिम्) भिनत्ति। महात्मा प्रह्लाद कहते हैं कि ऐसा जो भगवान आत्मा है सर्व का सर्व, वही मेरी बुद्धि को बिगाड़ता है। मेरी बुद्धि में यह भेद उसी का डाला हुआ है जो सर्व का सर्व है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त उसका ही स्वरूप है। सारे विश्व का जो 'मैं' है वही भगवान आत्मा मेरी बुद्धि को बिगाड़ता है और कौन बिगाड़ेगा?
'भगवान आत्मा के जानने में ज्ञाता को अनधिकार है और भगवान आत्मा को जानने में ज्ञाता को भी अनधिकार है।'
शब्द वही है, परन्तु भाव अलग-अलग है। यदि भगवान को आत्मा 'मैं' से भिन्न मानकर जानना चाहता है तो यह ज्ञाता की अनधिकार चेष्टा है और अपने आपको भगवान आत्मा से अभिन्न जानकर जानना चाहते हो तो जानेगा किसको? अतः यह भी ज्ञाता की अनधिकार चेष्टा है। एक में भी है और एक में भी नहीं है।
भगवान आत्मा मुझसे भिन्न है, इस ज्ञाता और भगवान 'मैं' हूँ, इस ज्ञाता को भी भगवान के जानने में अनधिकार है। वही भगवान आत्मा है, गुरुजी ! मेरी बुद्धि को बिगाड़ता है, जो बुद्धि की बुद्धि है, ज्ञान का ज्ञान है। जब महात्मा प्राहाद इस प्रकार अपने गुरुजी से कहे तो फिर गुरुजी का पारा एकदम चढ़ गया। उनका शरीर गुस्से से लाल हो गया और पाठशाला के किसी विद्यार्थी को बुलाकर कहने लगे कि कहाँ है मेरी बेंत, लाओ, इस मूर्ख प्रह्लाद को शिक्षा देनी होगी-
आनियतामरे वेत्रमस्काकमयशस्करः ।
कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धेश्चतुर्थोऽस्योदितो दमः ।।
दैतेयचन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रुमः ।
यन्मूलोन्मूलपरशोर्विष्णोर्नालायितोऽर्भकः ।।
(श्रीमद् भागवत 7, 5. 16. 17)
यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा है। इस दुर्बुद्धि, कुलाङ्गार लड़के को बिना दण्ड के होश न आएगा। बेंत के बिना होश ठिकाना न होगा। दैत्य वंश रूपी मलयागिरि चंदन के वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस चंदन वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करता है, यह नादान बालक उन्हीं की बेंठ बन रहा है, सहायक हो रहा है। प्रह्लाद का कान पकडे थप्पड़ भी लगाये, गाली भी देते हैं, परन्तु वहाँ दूसरा रंग चढ़ने वाला ही न था। दूसरा रंग चढ़ा ही नहीं।
कुछ दिन पाठशाला में पढ़ने के बाद किसी दिन प्रह्लाद की माता कयाधू ने सुंदर स्नान कराकर, सुंदर-सुंदर कपड़ों, गहनों से सुसज्जित करके प्रह्लाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप के पास प्रणाम करने को भेजा। प्रह्लाद ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप प्रेम से ओतप्रोत हो उसे गोद में बिठा लिया और पूछा-
प्रह्लादानूच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमम् ।
कालेनैतावताऽऽयुष्मन् यशिक्षद्गुरोर्भवान् ।।
(7 - 5 - 22)
बेटा प्रह्लाद ! पहिले तो तुमने कुछ अंड-बंड कहा था, अब शिक्षा पाकर आये हो तो तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया? जरा सुनाओ तो सही-प्रह्लाद कहते हैं-सुनिये पिताजी !
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ।।
(7-5-23)
यहाँ पर प्रह्लाद ने नवधा भक्ति का विवेचन किया है। अब इनके लक्षण सुनो-श्रवणं-भगवान की कथा को सुनना। कीर्तनं-भगवान के नाम का कीर्तन करना। स्मरणं-भगवान का स्मरण (ध्यान) करना। पादसेवनम्-भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चनं भगवान का पूजन करना। वन्दनं-उनकी स्तुति करना। दास्यं-भगवान का दास हो जाना। सख्यं-भगवान को अपना सखा मानना। और आत्मनिवेदनम्-भगवान हो जाना। यही नौ प्रकार की भक्ति है। ये सब भक्ति के लक्षण हैं, भक्ति नहीं। लोग आठ लक्षण तो बड़े प्रेम से सुनते हैं, परन्तु भगवान हो जाना यह सुनते ही मनीराम भागते हैं। और क्या-अरे बाप रे! हम भगवान कैसे हो जाएंगे-देखो-नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन है। भगवान की भक्ति दो प्रकार की होती है-एक परा भक्ति और दूसरी अपरा भक्ति। सगुण ब्रह्म की जो उपासना, उसे अपरा भक्ति कहते हैं और व्यापक निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना उसे परा भक्ति कहते हैं। अपरा भक्ति में भक्त और भगवान का भेद रहता है। सगुण उपासना, भेदोपासना, व्यक्तोपासना, परिच्छिन्न उपासना, भावनात्मक उपासना ये सब अपरा भक्ति के पर्याय हैं और निर्गुण उपासना, अव्यक्त उपासना, व्यापक उपासना, अभेद उपासना, अहंग्रह उपासना, ये सब परा भक्ति के पर्याय हैं। अपरा भक्ति या सगुण आराधना का आधार भावना है और भावना का फल है प्रेम। प्रेम का फल है भक्त भगवान की एकता और इस एकता का फल है चित्त की परम शांति। भगवान विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, शक्ति और गुरु, इनमें से जिनको भी व्यक्ति अपना भगवान माने, जो जिसका इष्ट हो, अपने उस इष्ट की मूर्ति को भावना द्वारा हृदय में स्थापित कर उसका ही मानसिक पूजन, अर्चन, वंदन, जप, नाम स्मरण, चिंतन एवं ध्यान करना यह अपरा भक्ति का स्वरूप है। यह भावना पर अवलंबित है। भावना का फल है प्रेम और प्रेम का फल है भक्त भगवान की एकता। एक हो गये। किस तरह ?
श्याम श्याम रटते रटते राधा श्याम भई ।
तब फिर पूछत यो सखियन से राधा कहाँ गई ।।
प्रेम जगत में भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। यदि भक्त, भगवान में भेद है, दो दिखाई देते हैं तो समझ लेना कि वह प्रेम की दुनियाँ से इतनी दूर है, जिसकी कोई सीमा नहीं। जब यह एकता इश्क मिजाजी में हो जाती है, आशिक माशूक एक हो जाते हैं तो फिर इश्क हकीकी में तो कहना ही क्या है। उपासक की दृष्टि में उपास्य (भगवान) यदि अलग दिखाई देता है, तो समझ जो कि वह सच्चा आशिक नहीं। प्रेम की दुनियाँ से वह बहुत दूर है।
अब दूसरी भक्ति है परा भक्ति-मैं व्यापक, परिपूर्ण, अखण्ड, अजर, अमर, निर्मल, निरंजन, निर्विकार, सनातन ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की भावना करने का नाम निर्गुणोपासना है। इसे ब्रह्मानुसंधान, अहंग्रह उपासना इत्यादि कहते हैं। इस उपासना का आधार विचार है।
कोऽहम् कस्त्वम् कुत आयातः । का मे जननी को मे तातः ।।
को मैं आयउँ कहाँ ते कित जइहौं का सार ।
का मे जननी को पिता याको कहत विचार ।।
परा भक्ति का आधार विचार है। इस विचार का फल है ज्ञान। जो व्यापक ब्रह्म परिपूर्ण है वही मैं हूँ। और जो मैं हूँ, वही तू है, फिर किसलिए पर्दा) इसका नाम है ज्ञान। इस ज्ञान का फल है जीव ब्रह्म की एकता। उपासक अपने आपको जीव मानकर ही उपासना करता है, परन्तु ज्ञान होने पर जीवात्मा का भेद निकल जाता है। एक ही हस्ती रह जाती है। तू है तो मैं नहीं और मैं हूँ तो तू नहीं। तू ही है, तू ही है या मैं ही हूँ, मैं ही हूँ भेद का सर्वथा अभाव हो जाता है। एक मुल्क में दो गवर्नमेंट नहीं हो सकती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हिन्दुस्तान और पाकिस्तान है। कभी भी सुख की नींद नहीं सो सकते। यह जो साढ़े तीन हाथ की दीवार vec 6 , इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तू रहे या मैं रहूँ। व्यापक ब्रह्म की उपासना अभेद है और यदि दो मानते हो तो अभेद भक्ति नहीं।
इन आँखों का यही विशेष, मैं तोहिं देखूँ तू मोहिं देख ।
देखत-देखत ऐसा देख कि मिट जाय दुविधा रह जाय एक ।।
कुदरत से आँख देखने को मिली है तो देख, आँख क्यों बंद करता है और ऐसा देख कि मिट जाये दुविधा रह जाय एक। ये बात-इसको परा भक्ति कहते हैं। यहाँ दो नहीं रहते। परा भक्ति का आधार विचार है और विचार का फल है ज्ञान। ज्ञान का फल है जीव और ब्रह्म की एकता जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिट जाना। इस एकत्व का फल है चित्त की परम शांति। परा भक्ति और अपरा भक्ति दोनों का फल एक ही है। चित्त की परम शांति दो में नहीं होती। अरे! दो में तो भय है। परा अथवा अपरा भक्ति में चित्त की शांति ही परम फल है। ध्यान दो-धारणा दो प्रकार की एक मार्जारी धारणा और दूसरी वानरी धारणा ? ॐशिव, भैया! तो मार्जारी धारणा के लक्षण जैसे बिल्ली की माँ अपने बच्चे को मुँह में दबाकर जहाँ जाना है, वहाँ ले जाती है। वे अपनी माँ h नहीं पकड़े रहते। माँ ही अपने दाँतों से बच्चों को पकड़ी रहती है। बिल्ली बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ है, जहाँ वह ले जाये। इस प्रकार की धारणा जहाँ भक्त की है, जहाँ भक्त पूर्णतया भगवान पर आश्रित है, उसे मार्जारी धारणा करते हैं।
दूसरी धारणा है वानरी धारणा-वानरी अपने बच्चे को नहीं पकड़ी रहती वरन् बच्चा ही वानरी के पेट भाग को अपने हाथों से ऊपर कसकर पकड़ा रहता है, ताकि जब उसकी माँ डालियों में कूदती-फांदती है तो वह गिर न जाय। वह स्वयं माँ से चिपटा रहता है। इसी प्रकार इस वानरी धारणा में भक्त मैं ही हूँ, यह धारणा रखता है और मार्जारी धारणा का उपासक (भक्त) तू ही है, तू ही है-यह भाव रखता है। तो फिर क्या सिद्ध हुआ? अगर तू ही तू है तो मैं नहीं और मैं ही, मैं हूँ, तो तू नहीं। इसी प्रकार परा और अपरा भक्ति को समझो, अब कुछ रामायण के पदों से इसका मार्जन कर दें। एक भक्ति ऐसी भी है कि जिसमें न मार्जारी भावना है, न वानरी। न अपरा भक्ति, न परा भक्ति- कोई नहीं, स्वतंत्र भक्ति है। जिस देश में न परा है, न अपरा। न निर्गुण, न सगुण। रामायण में सभी भावनाओं की भक्ति का निरूपण किया गया है। जरा इनका भी स्वाद लें। अपरा भक्ति के लिए चलें अरण्यकांड में-
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहिं कहँ जानै दृढ़ सेवा ।।
मम गुन गावत पुलक शरीरा । गद्गद गिरा नयन बह नीरा ।।
काम आदि मद दंभ न जाकें। तात निरंतर बस मैं ताके ।।
वचन कर्म मन मोरि गति भजन करहिं निष्काम ।
तिन्हके हृदय कमल महुँ करुउँ सदा विश्राम ।।
यह अपरा भक्ति है-सगुण भगवान की उपासना और-
सो तैं ताहि-तोहि नहिं भेदा। वारि वीचि इव गावहिं वेदा ।।
सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि ।
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धान्त विचारि ।।
यहाँ परा भक्ति है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर तो सभी रामायण के प्रकाण्ड विद्वान (पंडित) बैठे हो। सुनो, इसका भाव-सेवक, सेव्य भाव बिनु भव न तरिय-अपरा भक्ति। बिना सेवक सेव्य भाव के संसार से नहीं तरता। सेव्य भाव बिनु, सेवक, भव न तरिय-परा भक्ति। सेवक में जब तक सेव्य भाव नहीं आ जाता तब तक वह नहीं तरता। सेवक सेव्य भाव विन भवन न-स्वतंत्र भक्ति। सेवक-सेव्य भाव के बिना भव (संसार) नहीं है। अस सिद्धान्त विचारि राम पद पंकज भजहु। ऐसा विचार करके भगवान राम के चरण-कमलों को भजो। प्रणाम ?
सोई जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हई होइ जाई ।।
सेव्य भाव हो गया कि नहीं?
श्वेताश्वतरोपनिषत् की एक श्रुति स्पष्टतया बतलाती है कि जीव के आवागमन का कारण क्या है? कैसे ?
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे वृहन्ते तस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ।
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ।।
(1.6)
प्रेरितारं परमात्मानं आत्मानं पृथक् मत्वा तस्मिन् ब्रह्मचक्रे संसारे हंसो जीवः भ्राम्यते जुष्टः ततः तेन् अमृतत्वं एति प्राप्नोति इति भावः ।
परमात्मा भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार मानकर ही जीव ब्रह्मचक्र संसार में भ्रमाया जा रहा है। इस प्रकार की मान्यता ही जीव के चौरासी लाख योनियों में भटकने का एकमात्र कारण है।' जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति'- जब यह जीव परमात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा को अपने स्वरूप से भिन्न नहीं जानता तब यह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है अर्थात् आवागमन के चक्र से छूट जाता है। तो फिर परमात्मा के साथ जीव का जुड़ना क्या है? इधर से परमात्मा आये, उधर से जीव, दोनों एक जगह जुड़ गये? जोड़ का अर्थ यह नहीं है। तो फिर क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा कहना क्या परमात्मा से जुड़ना है? नहीं, यह जुड़ना नहीं है। यदि भगवान अपने आप को भगवान कहे तो मैं भी अपने आपको भगवान कहूँ और यदि भगवान अपने आपको भगवान भी नहीं कहता तो मुझको क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं अपने आपको भगवान कहूँ या भगवान मानूँ, यह भी जंजाल है। भगवान का भगवान नाम किसने रखा? भगवान ने रखा कि भक्तों ने? भगवान नाम भक्तों ने रखा है। इसलिए इसे भगवान कहते हैं कि वह अपने आपको भगवान नहीं कहता। कोई न कोई विलक्षण तत्व है-क्या रहस्य है? जब 'मैं' भगवान आत्मा पर यह भी मान्यता रही कि मैं भगवान हैं तब 'मैं' का 'मैं' शुद्ध तत्व ही रह जायेगा। यह जोड कभी टूटने वाला नहीं है। शिव-भैया ! इसलिए 'सेवक सेव्य भाव विक जोड़ तरिय उरगारी।' जब आ गया सेव्य भाव तो अस सिद्धांत विचारि राम पद पंकज भजहु। यह परा भक्ति है।
एक निराली भक्ति और है, जो कि न परा है और न अपरा। तो फिर वह कौन-सी भक्ति है?
पावन पर्वत वेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना ।।
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी । ग्यान विराग नयन उरगारी ।।
माताजी ने प्रश्न किया कि-
नर सहस्त्र महँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होई धर्मव्रतधारी ।।
धर्मशील कोटिक महँ कोई। विषय विमुख विराग रत होई ।।
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक् ज्ञान सकृत कोउ लहई ।।
ग्यानवन्त कोटिक महँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ।।
तिन्ह सहस्त्र महँ सब सुखखानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ।।
सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ।। तो फिर वह कौन सी भक्ति है जिसमें रत होने पर मद और माया गत हो जाते हैं और वह भक्ति प्राप्त कैसे होती है?
सो हरि भगति काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहिं कहहु बुझाई ।।
वह कौन-सी भक्ति है? अपराभक्ति भावना प्रधान है-भावना की जाती है कि मैं भक्त हूँ और पराभक्ति में भावना की जाती है कि मैं ब्रह्म हूँ। मान्यता दोनों में है। परा भक्ति का अधिकारी इस भाव में रहता है कि मैं सनातन ब्रह्म हूँ और तुलसीदास जी कहते हैं, वह भक्ति कैसी है?
राम भगति रत गत मद माया। कभी सोचा है? मानस प्रेमियों !
वह कौन सी भक्ति है?
पावन पर्वत वेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना ।।
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ग्यान विराग नयन उरगारी ।।
भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी ।।
ज्ञान वैराग्य से परे भक्ति-तो फिर वह कौन-सी भक्ति है जिसकी तरफ श्री तुलसीदास जी निर्देश कर रहे हैं?
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई ।।
वह कौन-सी भक्ति है, जरा विचार करो-
सो स्वतंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ग्यान विग्याना ।।
वह भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान की उपेक्षा करने वालों को ध्यान से सुनना चाहिये।
सो स्वतंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ग्यान विग्याना ।।
वाह भाई वाह ! भक्ति कहो या आत्मा-यह तो संतों, महापुरुषों ने, आत्म तत्व को भक्ति नाम से विभूषित किया है-और फिर इस भक्ति का क्या स्वरूप है? हाँ-कोई आधार-अवलंब तो होना चाहिए। जिस भक्ति के अधीन ग्यान विग्यान है-'तेहि आधीन ग्यान विग्याना।' ज्ञान विज्ञान का क्या स्वरूप है और दोनों जिसके आधीन हैं वह भक्ति क्या है? अहँ ब्रह्मास्मि-मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान है। अहमेवेद् सर्वम् - मैं सर्व हूँ यह विज्ञान है या मैं आत्मा का आधार ब्रह्म है? मैं सर्व हूँ, इसका आधार मैं आत्मा का आधार सर्व है? ज्ञान और विज्ञान दोनों का आधार 'मैं' आत्मा हूँ।
सो स्वतंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ग्यान विग्याना ।।
भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलहिं जो संत होहिं अनुकूला ।।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ।।
उस भक्ति का क्या स्वरूप है जो सकल सुख खानी है? तो यहाँ पर जानना चाहिए कि भक्ति है- 'मैं' पद, कैवल्य पद, आत्म पद और यह साधन का विषय नहीं है। यह कोई बाजारु चीज नहीं है। श्रीमानसकार कहते हैं- ऐसी जो स्वतंत्र भक्ति है उसके लिए सत्संग ही साधन है।
सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाई ।।
तो भैया !
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी।
और-
भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलहिं जो संत होहिं अनुकूला ।।
क्यों नहीं पढ़ते इन चौपाइयों को-संत मिलें और फिर संत अनुकूल हो। लाख जतन करो, साधन करो, परन्तु उनसे स्वतंत्र भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती इसलिए संत कृपा का भिखारी बनो। हाँ-साधन करने से संत कृपा का अधिकारी है। संत कृपा से ही भगवान आत्मा आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में संत कृपा ही साधन है।
संत विशुद्ध मिलहिं परि तेही। चितवहिं राम कृपा करि जेही ।।
जिन संतों की कृपा से आत्मतत्व का बोध प्राप्त होता है, परम पद, कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, जिसको कि स्वतंत्र भक्ति कहते हैं, वे संत कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होती है तो संत मिलते हैं और संत कृपा का फल है परम पद की प्राप्ति । भगवान की भक्ति मिलती है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, संत कृपा कहो या भगवत् कृपा कहो, एक ही पहलू के दो नाम हैं, संत कहो या भगवान। जी हाँ-
मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार दिया ।।
मन मारा तन वश में कीन्हा भरम भये सब दूर ।
बाहर से कछु दीखत नाहीं अंदर बरसे नूर ।। जिन्होने.
आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम ।
उनमें से कछु अंतर नाहीं संत कहो चाहे राम ।। जिन्होंने.
पी लिया प्याला ज्ञान का छोड़ जगत का मोह ।
हमको सतगुरु ऐसे मिल गए होनी होय सो हो ।। जिन्होंने.
नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया अमिय रस प्याय ।
एक बूंद सागर में मिल गई कहा करैगा यमराय ।। जिन्होंने.
भैया! ऐसे संतों से ही भक्ति, आत्म पद प्राप्त होता है।
नानक निदरी निदर निहाल ।
संतों के दृष्टि मात्र से कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कन्ध में भगवान श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हैं-
निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् ।
अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ।।
(11-14-16)
जो संत निरपेक्ष हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं निर्देर है अर्थात जिनका कोई शत्रु मित्र नहीं, जो शांत हैं और समदर्शी अर्थात् सारे विश्व को अपना ही स्वरूप आत्मा देखने वाले हैं, तो अहं अनुव्रजामि-मैं नित्य उन संतों के पीछे-पीछे घूमता रहता हूँ। किसलिए? पूयेयेतङ्घ्रिरेणुभिः इसलिये कि उनके चरणों की धूल मुझ पर पड़ जाय तो मैं पवित्र हो जाऊँ।
संत विशुद्ध मिलहिं परि तेही। चितवहिं राम कृपा करि जेही ।।
राम कृपा से संत का मिलन और संत मिलन से आत्म दर्शन (अनुभूति) भगवान की भवहरणि भक्ति मिलती है-जो भक्ति स्वस्वरूप भगवान आत्मा अपना आप है। जी हाँ-राम कृपा से ही आत्मानुभूति होती है। इसका पर्यायवाची नाम है परम प्रकाश। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को परम प्रकाश कहा है-
परम प्रकाश रूप दिन राती। नहिं कछु चहिये दिया घृत बाती ।।
यही आत्मपद, कैवल्यपद, तूष्णीपद, सत्ता पद एवं परम प्रकाश है। यह प्रकाश दिया, घृत, वाती अर्थात् साधनवाला नहीं है।
सोऽहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा ।।
परम प्रकाश साधनसाध्य नहीं है। यह तो संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। साधन द्वारा दिया, घृत, बाती का प्रकाश प्राप्त होता है। इस दिया को हवा बुझा सकती है।
आवत देखहिं विषय बयारी। ते हठि देहिं कपाट उघारी ।।
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई ।।
आदि। जो परम प्रकाश है वह क्या हवा से बुझेगा? क्या सूर्य का प्रकाश हवा से बुझेगा? दिया तो बुझ जाएगा। परम प्रकाश जो कि प्रकाश को भी प्रकाशित करता है वह संत कृपा का फल है।
परम प्रकाश रूप दिन राती। नहिं कछु चहिय दिया घृत बाती ।।
देखो, समझो विषय-रात्रि के निविड़ अंधकार में खड़े हो और कहते हो- बड़ा काला अंधेरा छाया हुआ है, अपना हाथ भी नहीं सूझता। भैया ! जल्दी टार्च लाओ, कन्डील लाओ, बड़ा काला अंधेरा है। तो प्यारे ! उस काले काले अंधकार को तुम किस प्रकाश से देख रहे हो-सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश तो इस अंधकार का प्रतिद्वंद्वी है, उसका नाशक है इसलिए इन प्रकाशों द्वारा तो रात्रि का घोर अंधकार नहीं दिखेगा। तो फिर तुम किस आँख से किस प्रकाश से रात्रि के अंधकार को देख कर कहते हो कि बड़ा अंधकार है. हाथ से हाथ नहीं सूझता। सौम्य । वह कौन-सा प्रकाश है जिससे रात्रि के अंधकार को देखते हो? और सुनो-रात्रि में जब तुम सो जाते हो तो सारी इन्द्रियाँ शिथिल पड़ी रहती हैं, आँख बंद रहती है और स्वजाते नानात्व का अनुभव करते हो, दिन सा कार्य करते हो, जाग्रत अवस्था के जैसा सभी कार्य करते हो जबकि सूर्य, चन्द्रमा किसी का प्रकाश नहीं रहता, तो वह कौन-सा प्रकाश है जिसके द्वारा, जिस प्रकाश से रात्रि के स्वप्न में जाग्रत जैसा व्यवहार देखते हो? जाग्रत का प्रपंच स्वप्न में कैसे देखते हो? यह किस प्रकार से संभव हुआ? अरे ! जिस प्रकार से दिन का व्यवहार करते हो वही, उसी प्रकाश से रात्रि का स्वप्न भी देखते हो।
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्रिः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।।
(मु. 2-2-10)
जिसे सूर्य का प्रकाश, चन्द्र का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता जो स्वयं इस परम प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तो वह कौन-सा प्रकाश है जिसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारागण, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती? गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।।
(गीता 15-6)
भगवान यहाँ भी वही कह रहे हैं। गत्वा धातु के चार अर्थ- गम्-गत्वाः - प्राप्त कर, जानकर, पहुँचकर और मोक्ष। 'यदगत्वा न निवर्तन्ते' जहाँ जाकर फिर नहीं लौटता, मोक्ष हो जाता है, वही आत्मा 'मैं' हूँ। इसका मतलब यही हैन कि भगवान की कोई कोठी है, कोई धाम है जहाँ वे रहते हैं। 'मैं' आत्मा हैं। परम प्रकाश हूँ, परम प्रकाश रूप दिन राती। जो जाग्रत के प्रपंच को देख रहा है, जो स्वप्न के प्रपंच को देख रहा है, जो सुषुप्ति अवस्था का साक्षी है, वह कौन है? मैं आत्मा, दूसरा कौन होगा सिवाय मुझ आत्मा के। इसलिए 'मैं' साक्षी हूँ। मुझमें प्रपंच नहीं है। जो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति का अनुभव करता है, वही परम प्रकाश है। 'मैं' अभी हूँ तो क्या 'मैं' रात्रि में न रहूँगा। नहीं 'मैं' रात्रि में भी रहूँगा। दिन के प्रकाश का मैं प्रकाशक हूँ और रात्रि के अंधकार का भी प्रकाशक हूँ। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों को जानता हूँ। देखो-आज सुबह जब तुम उठे तो क्या बजे थे? 6 बजे थे। सुबह के 6 बजे को किसने जाना? 6 बजे काल में मैं आत्मा था कि नहीं? था। तभी तो 6 बजे को जाना। उस समय उठा इसका अनुभव किया। भैया! यहाँ पर साहित्य का कथन नहीं होता। यहाँ पर तो ब्रह्म सूत्रों एवं चारों वेदों के जो भाव निकलते हैं, उसका निरूपण एवं साक्षात्कार कराया जा रहा है। 6 बजे वाले काल को मैं आत्मा न होता तो कौन देखता। फिर 7 बजे वाला काल आया और चला गया। फिर 8 बजे वाला काल 10, 11 काल धड़ाधड़ आया और चला गया। काल वेग बड़ा विलक्षण है। अत्यंत वेग वाला है। वर्तमान भूत हो रहा है और भविष्य क्षण-प्रतिक्षण वर्तमान होता जा रहा है। वाणी की ताकत नहीं कि इस वेग को अभिव्यक्त कर सके कि इस काल की कितनी गति (स्पीड) है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसका वेग कितना है? विज्ञान बड़ा वेगशाली राकेट का निर्माण किया है। रूस और अमेरिका क्या-क्या विज्ञापन करते हैं, लाखों मील की स्पीड बताते हैं। परन्तु काल भगवान के सामने सबों की गति धीमी ही है। काल जो सबको खाता है, उसको महाकाल भगवान आत्मा मैं खाता हूँ।
जो कालहु कर काल भयंकर। वरनत उमा सारदा शंकर ।।
तो मैंने 7 बजे वाले काल को खाया। 9, 10, 11 बजने वाले कालों को खाया, 6 बजे शाम वाले काल को खाऊँगा, फिर आत्मा कालातीत कहलाता है।
परम प्रकाश रूप दिन राती। नहिं कछु चहिय दिया घृत बाती ।।
यहाँ दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। सबका प्रकाश 'मैं' आत्मा हूँ। ज्ञान दीपक साधन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाय वह जब तक परम प्रकाश रूपी भक्ति को न प्राप्त कर ले-अधूरा है। परम प्रकाश भगवान आत्मा चिंतामणि है। तो चिंतार्माण क्या है? महारामायण (योगवाशिष्ठ) के निर्वाण प्रकरण में जब श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को आत्मा का स्वरूप बता रहे थे, वहाँ बतलाते हैं कि आत्म तत्व चिंतामणि हैं। चिंतामणि को जिस रूप में देखना चाहते हो उसी रूप में दिखाई देता है। यदि अपने आपको साढे तीन हाथ का मानते हो तो उसे भगवान आत्मा साढे तीन हाथ का ही है, ऐसा दिखता है। जो अपने आपको जीव मानता है उसे व्यापक ब्रह्म, ब्रह्मा से तुण पर्यन्त अपना ही स्वरूप दिखता है, क्योंकि भगवान आत्मा चिंतामणि है।
राम भगति चिंतामणि सुंदर। बसइ गरुड़ जाके उर अंतर ।।
नारद जी भक्ति सूत्र में बतलाते हैं कि भगवान की भक्ति, महात्माओं (संतों) और भगवान की कृपा से मिलती है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि जो भक्ति है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या साधन है?
मुख्य तस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपा लेशाद्वा।
महत्सङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च । लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव ।।
(ना.भ.सू. 38, 39, 40)
संतों महापुरुषों का संग, बड़ा ही दुर्लभ एवं अगम्य होता है और यदि प्राप्त हो जाय तो अमोघ होता है। लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव- भगवान की जब कृपा होती है तभी वे संत मिलते हैं, जिनकी कृपा से भगवान की चिंतामणि रूपी भक्ति प्राप्त होती है।
संत विशुद्ध मिलहिं परि तेही। चितवहिं राम कृपा करि जेही ।।
का भाव लग गया न? तो फिर उन संतों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिये जिन संतों की कृपा से भक्ति (आत्म पद) मिलता है? तो कहते हैं-
तस्मिस्तज्जने भेदाभावात् ।।
(ना.भ.सू. 41)
उस संत में और भगवान में भेद का अभाव रहता है। यानी उस संत के प्रति हमारे हृदय में जब नारायण भाव होगा तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा। आत्म कल्याण नर से नहीं होता। नर बेचारा नारायण तक क्या पहुँचाएगा- खुद ही जो गरीब है वह क्या अमीर बनाएगा। नारायण से ही नारायण मिलते हैं और नारायण, नारायण से ही मिलते हैं। जीव बेचारे की क्या पहुँच है जो कि स्वयं गरीबी ढो रहा है। नारायण, नारायण को ही मिलेगा।
तदेव साध्यतां तदेवसाध्यताम् ।।
(नाभसू 42)
भगवत्प्राप्ति के लिए अगर साधन करना है तो संतों के मिलने का साधन करो। संतों को ही साधो जिसकी कृपा से भगवान आत्मा का दर्शन होता है। साधन करना है तो संत दर्शन का साधन करो-भगवान तो तुम स्वयं ही हो। जो आत्मा सर्व का सर्व है, उसको साधन से कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए किसी महान पुरुष की शरण में जाने का साधन करो। जिसकी शरण में जाने से, जो कृपा करके, करुणा करके भगवान को प्राप्त करा देते हैं। महान पुरुषों की आत्मतत्व को लखाने की प्रक्रिया विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। वे जिज्ञासुओं को करुणा करके आत्म पद, कैवल्य पद, निर्वाण पद अर्थात् स्वतंत्र भक्ति प्रदान करते हैं। यही स्वतंत्र भक्ति का स्वरूप है। फिर देखो-भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक के अवसर पर चारों वेद भगवान के दर्शन हेतु गये थे। वे बन्दी रूप से भगवान की स्तुति करते हैं-
जे ज्ञान मान विमत्त तब भय हरणि भक्ति न आदरी ।
ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि पतत हम देखत हरी ।।
(रामायण)
जो माने हुए ज्ञान के भाव में उन्मत्त होकर भगवन् ! आपकी भवहरणि भक्ति का आदर नहीं करते, उनका सुरदुर्लभ पद निर्विकल्पावस्था को पाकर भी पतन होते देखा है। अहंब्रह्मास्मि- मैं ब्रह्म हूँ, यह माना हुआ ज्ञान है कि जाना हुआ। अब भवहरणि भक्ति क्या है? अरे, जहाँ पर अहँ ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हूँ) इस अज्ञान नाशक माने हुए ज्ञान का भी नाश हो जाता है वही भवहरणि भक्ति (आत्म पद) है। आत्म देश में संसार नाम की कोई चीज नहीं है। आत्म पद भैया ! वह पद है, जिसमें और कोई विकार नहीं। शुद्ध तत्व 'मैं' का 'मैं' यही भवहरणि भक्ति है। जो इसका समुचित आदर नहीं करते, उसको देव दुर्लभ पद को प्राप्त करके पतन होते देखा है। देखो-तुम्हें क्या चीज समझा दूँ, तृप्ति नहीं होती यार! अघाते नहीं है।
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।।
(गीता 7 - 19)
बहुनां जन्मनां अन्ते जन्मनि-ज्ञानवान् माम् आत्मानं प्रपद्यते। नीचे का चरण इसकी फलश्रुति है। बहुत जन्मों के अन्त वाले जन्म में ज्ञानवान मुझ आत्मा को प्राप्त करता है। अन्ते जन्मनि-आगे अब उसको जन्म लेना नहीं है। उस ज्ञानवान का वह आखिरी जन्म होगा। अन्ते जन्मनि ज्ञानवान् भवति अथवा ज्ञानवान् माम् आत्मानं प्रपद्यते-अन्त वाले जन्म में ज्ञानवान होता है अथवा ज्ञानवान मुझ आत्म को प्राप्त होता है? यदि बहुत जन्मों के अन्त वाले जन्म में ज्ञानवान होता है तो फिर प्राप्त कौन से जन्म में करेगा और बिना मुझ आत्मा को जाने, जन्मों का अन्त नहीं होता। जो-जो ज्ञानवान है वह अपने आप को क्या लक्ष्य करता है, उसका लक्ष्य क्या है? अहं ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ इस प्रकार की धारणा वाला ज्ञानवान कहलाता है। मैं ब्रह्म हूँ, इस धारणा का पुरुष ज्ञानवान हुआ। तो फिर जन्म का अन्त नहीं हुआ। भगवान के कथन से मालूम होता है कि जब वह अपने आप 'मैं' आत्मा को प्राप्त कर लेता है तभी उसके जन्मों का अन्त होता है।
'वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः' वासुदेव सर्वमिति, इस सिद्धांत पद में स्थित महात्मा संसार में दुर्लभ हैं। समझो, प्रत्येक विषय के निश्चयात्मक भाव को प्राप्त करने के लिए चारों प्रमाणों से जो प्रमाणित हो वही वास्तविक भाव होगा।
प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा ।
आद्यन्तवतसद् ज्ञात्वा निःसंगो विचरेदिह ।।
प्रत्यक्ष, अनुमान, निगम और स्वानुभूति, इन चारों प्रमाणों से जो सिद्ध हो वही वास्तविक भाव होगा। सारांश यह है कि इस आत्म पद, कैवल्य पद, भक्ति स्वरूप, परम प्रकाश देश में न परा, न अपरा भक्ति, न वानरी न मार्जारी धारणा, न व्यक्त, न अव्यक्त उपासना। सूर्य देश में जिस प्रकार सूर्य ही है, सूर्य के अतिरिक्त दूसरी सत्ता ही नहीं है, इसी प्रकार मुझ आत्मदेश में सिवाय मुझ आत्मा भगवान 'मैं' के दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। यही कृत कृत्य पद है, कैवल्य पद हैं। भगवान पतंजलि योग दर्शन में दर्शाये हैं-
विशेष दर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्तिः ।।
(योग.सू. कैवल्य पाद)
महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्वरूप का पूर्ण बोध (अनुभव) हो जाने पर आत्मभाव की भावना की भी निवृत्ति हो जाती है। आत्मभाव की भावना क्या है? अहं ब्रह्मास्मि - मैं ब्रह्म हूँ, कूटस्थ हूँ, साक्षी हूँ, अजर-अमर, अखण्ड, अपार, निर्मल, निरञ्जन, निर्विकार हूँ इत्यादि। मैं आत्मा पर इस प्रकार की भावना की जाती है। जब स्वरूप भगवान आत्मा 'मैं' का बोध हो जाता है तब शुद्ध तत्व 'मैं' का 'मैं' रह जाता है।
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ।।
इस प्रकार जब प्रह्लाद ने हिरण्यकश्यप से कहा तो हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो गया और क्रोधातुर हो कहता है कि इस छद्मवेशी ब्राह्मण ने मेरे पुत्र प्रह्लाद को बिगाड़ दिया है।
ब्रह्मबन्धो किमेतते विपक्षं श्रयतासता ।
असारं ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते ।।
(श्रीमद् भागवत 7-5-26)
गुरु पुत्र शण्डामर्क को कहता है कि तुम सब ब्राह्मणों ने पुत्र को बिगाड़ दिया है। गुरुपत्र शण्डामर्क ने कहा कि हे राजन् ! इसकी बुद्धि को हम लोगों ने नहीं बिगाड़ा है, हमें तो ज्ञान क्या है एवं भक्ति क्या है यह भी पता नहीं। इसकी बुद्धि नैसर्गिक है। सदैव मन ही मन यह ऐसा ही गुनगुनाता रहता है, न मालूम कौन है कि जो अंदर ही अंदर इसकी बुद्धि को बिगाड़ रहा है।
न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो ।
नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्नियच्छ मन्युं कददाः स्म मा नः ।।
(श्रीमद् भागवत 7.5.28)
हिरण्यकश्यप गरज कर बोलता है कि ऐ दबुद्धि बालक। गुरु पुत्र क्या कहते हैं? तेरी बुद्धि को तेरे दिमाग को कौन बिगाड़ रहा है? तो महात्मा प्रह्लाद कहते हैं-
मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम् ।
अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रं पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम् ।।
(श्रीमद् भागवत 7.5.30)
न ते बिदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः ।
अन्धा यथान्यैरुपनीयमाना वाचीशतन्त्यामुरुदाम्नि बद्धाः ।।
(श्रीमद् भागवत 7.5.31)
नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रि स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः ।
महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् ।।
(श्रीमद् भागवत 7.5.32)
जिनकी बुद्धि भगवान श्रीकृष्ण आत्मा में संलग्न नहीं है, जो गृहव्रती अर्थात् जो दारासक्त, पुत्रासक्त, वित्तासक्त है, वे उन पशुओं के समान हैं जो चबाये हुए को चबाते हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी शुभाशुभ घटनायें हो चुकी हैं, उन्हीं का कथन, वे अपने समाज में, मित्रवर्गों में एवं जहाँ कहीं भी बैठते हैं, करते हैं। विद्वानों द्वारा सकाम कर्म करने की वाणी को सुनकर जो परम स्वार्थ भगवान विष्णु को नहीं जानते, उनके विमुख हैं ऐसे दुराशयी अर्थात् इहलोक परलोक के पदार्थों को प्राप्त करने की आशा से सकाम कर्म करने वाले हैं, उनकी बुद्धि पहले की अपेक्षा और भी दृढ़तापूर्वक सकाम कर्म करने में संलग्न हो जाती हैं। जिस प्रकार अंधे को अंधा रास्ते पर ले जाय उसी प्रकार अनुभव शून्य संसारी विद्वानों की सकाम कर्म करने की वाणी रूपी रस्सी द्वारा अज्ञानी संसारी जीवों की बुद्धि बंधी रहती है। उनकी बुद्धि इतनी स्थूल हो बाती है कि सूक्ष्म तत्व भगवान आत्मा का विचार करने में समर्थ नहीं हो सकती।
यावत् निष्किञ्चनानां महीयसां पादरजोऽभिषेकं न वृणीत तावत् ।।
"उरुक्रमाङघ्रि भगवच्चरणं न स्पृशति' जब तक निष्किञ्चन वीतराग महान पुरुषों के चरण कमलों की वह रज का अभिषेक नहीं हो जाता तब तक भगवान के चरणकमलों का वह स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान की भवहरीत भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे साकार ब्रा का दर्शन हो या निराकार व्यापक ब्रह्म का, संत कृपा ही साधन है। संत कृपा पर ही भगवत् दर्शन अवलम्बित है।
हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद की इस प्रकार की भक्तियुक्त वाणी को सुना तो वह क्रोध से उन्मत हो गया और प्रह्लाद को गोद से उठाकर नीचे पटक दिया। क्रोध के आवेश में सेवकों से कहा- इस कुलाङ्गार को ले जाओ।
वध्यतामाश्वयं वध्यो निःसारयत नैर्ऋताः ।।
(श्रीमद् भागवत 7 - 5 - 34)
सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः संभोजशयनासनैः ।
सुहृल्लिङ्गधरः शत्रुर्मुनेर्दुष्टमिवेन्द्रियम् ।।
(श्रीमद् भागवत 7-5-38)
ले जाओ इसे, मार डालो, विष दे दो, जो कि इस छोटी-सी उम्र में हमारे शत्रुपक्ष की बात कर रहा है। यह मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है। जाओ ! इसे पहाड़ पर से गिरा दो। जब शरीर में कहीं रोग हो जाये और उससे सारे अंग की हानि की आशंका हो तो उस भाग को काटकर अलग कर देना चाहिये। शरीर का फोडा सारे शरीर को नष्ट कर देता है, इसलिए उस अंग को काटकर फेंक देना चाहिये, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर तो सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर कोई मेरा शत्रु ही आया है। इसलिए तुरंत इसे ले जाओ और समुद्र में डुबा दो, आग में जला दो। हिरण्यकश्यप इस तरह से प्रलाप करने लगा। दैत्यगण द्वारा प्रह्लाद, जो अभी केवल 7 वर्ष का है-को मारने के सभी उपाय किये गये, परन्तु प्रह्लाद का कुछ भी न बिगाड़ सके। वे क्रोधपूर्वक प्रह्लाद को नाना प्रकार से प्रताड़ित किये, शूल से मारने लगे, परन्तु प्रह्लाद अडिग रहे। मन, वाणी से अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार परब्रह्म में जिसका चित्त अडिग है उसके सामने कौन-सी शक्ति है जो कि उसका कुछ भी अहित कर सके। दैत्यों के सभी प्रयास वैसे ही निष्फल हो गए जैसे- भाग्यहीनों के मनोरथ। प्रह्लाद को मतवाले हाथी से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी द्वारा भी वध करने का प्रयत्न किया गया, माया से अंधकार पैदाकर प्रह्लाद को अंधकार में रखा गया, विष दिया गया, दहकती आग में डाल दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, परन्तु किसी भी उपाय से निष्पाप प्रह्लाद का बाल बांका न हुआ। प्रह्लाद की मृत्यु न हुई। कारण, क्यों मृत्यु न हुई? मृत्यु कैसे हो? अरे ! जिसकी दृष्टि में मृत्यु भी भगवान आत्मा है तो मृत्यु कैसे हो? आत्म जिज्ञासुओं ! आत्म तत्व का कितना प्रभाव है, यह कितना सुदृढ़ कवच है। इसके सामने एटम बम, हाइड्रोजन बम सभी फेल हो जाते हैं सिर्फ आँख बदलने की बात है। भगवान आत्मा को जानना ब्राह्मी दृष्टि प्राप्त कर लेना, राग-द्वेष की आँखों को बदल देना है। अरे! करना कुछ नहीं है, केवल दृष्टि ही बदलनी है। देखो-
दो बालक-बालिका बचपन से एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं। साथ-साथ पढ़ते हैं। एक ही गुरु के पास दोनों शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रायमरी क्लास में साथ पढ़े, फिर हाई स्कूल में साथ ही पढ़े और कॉलेज में भी साथ-साथ ही पढ़े। इस तरह वयस्क होते एक-दूसरे को आपस में किस दृष्टि से देखते रहे? भाई और बहन के रूप में। अब कुछ समय बाद उनमें प्रेम हो गया और शादी हो गई। भांवर पड़ते ही कौन-सा भाव उदित हो गया? क्या वह पहले वाला भाई-बहन का भाव रखते हैं? नहीं, वह पुरानी दृष्टि नहीं रही, वह बदल गई और अब पति-पत्नी की दृष्टि हो गई। एक-दूसरे को पति-पत्नी देखने लगे, दृष्टि बदल गई। शादी होते ही पति-पत्नी का भाव आ जाता है। यद्यपि उनका शरीर तथा रूप रंग वही, परन्तु दृष्टि बदल गई। अज्ञानी की दृष्टि में यह संसार है। भेदवादियों ने संसार दृष्टि दृढ़ कर दिया है। तू छोटा है, वह बड़ा है। तू संसारी है, बद्ध है, जीव है, तू कैसे ईश्वर तत्व होगा-परन्तु बोधवान, भगवान वासुदेव आत्मतत्व ही देखता है, सभी भगवान है। आप सहित सबको भगवान आत्मा जानता है। बस ! इतना ही तो करना है और क्या-
गजेऽपि विष्णुर्भुजगेऽपि विष्णुर्जलेऽपि विष्णुज्र्ध्वलनेऽपि विष्णुः ।
त्वयिस्थितो दैत्यमयिस्थितश्च विष्णुं बिना दैत्यगणोऽपि नास्ति ।।
यही महात्मा प्रह्लाद की भगवद्भारणा थी। हाथी में भगवान, हाथी स्वयं भगवान। सर्प में भगवान, सर्प स्वयं भगवान, जल में भगवान, जल स्वयं भगवान, अग्नि में भगवान, अग्नि स्वयं भगवान। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सारा चराचर भगवान है। दैत्यगणों! तुम्हारे अंदर भगवान और मेरे अंदा भगवान, तुम स्वयं भगवान और मैं स्वयं भगवान। भगवान विष्णु से भिन्न कुछ भी नहीं। स्वामी जी ! हाँ जी, बात तो आपने ठीक ही कही कि सब कुछ भगवान है। भाई ! तो खराबी कहाँ रह गई, इसमें शंका की क्या बात है? यदि तुम्हें कोई शंका हो तो कहो। नहीं, स्वामी जी। ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ, घबराने की क्या बात है, घबराते क्यों हो? जब स्वामी जी ! सभी भगवान है ऐसी दृष्टि हो जायेगी तो फिर संसार में व्यवहार कैसे चलेगा? भैया। यह तो तुम्हारी बड़ी भारी शंका है। हम इसका मतलब बतलायें? अभी जो तुम व्यवहार कर रहे हो-चला रहे हो वह नर होकर व्यवहार कर रहे हो या नारायण होकर ? अभी जो व्यवहार कर रहे हो वह नारायण दृष्टि से कर रहे हो या नर दृष्टि से? चुप क्यों हो? बोलो ना यार। नर दृष्टि से कर रहे हैं। यदि वही व्यवहार तुम नारायण दृष्टि से करोगे तो क्या अंतर पड़ेगा? अभी तक नर दृष्टि से व्यवहार करते रहे हो अभी उसी व्यवहार को नारायण दृष्टि से करो। मैं भी भगवान और वह भी भगवान। देखो, माता-पिता की सेवा कैसे करते हो- नर होकर या पशु होकर? तुम कौन हो? मनुष्य। और तुम्हारे माता-पिता कौन हैं? वे भी मनुष्य हैं। मनुष्य होकर ही मनुष्य की सेवा कर रहे हो और सभी यही कहते हैं। माता-पिता को भगवान जानकर सेवा करना और अपने को भी भगवान ही जानना, यह भगवान द्वारा भगवान की सेवा हुई। जब तक तुम्हारी दृष्टि में राग-द्वेष है, हृदय विकारों से भरा हुआ है तब तक आवागमन का चक्र चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। अच्छा, देखो-अभी तुम्हारी शंका का समाधान हो जायेगा। अंग्रेजी शब्द गॉड से क्या बना-ईश्वर और इसी को उलट दो तो फिर क्या होगा-डॉग ! डॉग माने कुत्ता। सिर्फ दृष्टि उलटनी है, पशु से भगवान हो जाओगे।
एक कहीं का जमींदार जो काफी धनवान था, शीशमहल बनवाया। दीवाल शीशे का, खंभे भी शीशे के, फर्श भी शीशे का, छत भी शीशे की, सभी शीशे का ही बनवाया। फिर चारों तरफ खिड़की दरवाजे सब मोटे-मोटे काँच के बनवाये। इस आलीशान मकान में जाकर वह बीचोंबीच खड़ा हो गया और क्या देखता है कि चारों तरफ उसका ही प्रतिबिम्ब और प्रतिबिंब के प्रतिबिंब, हजारों की तादाद में अपने आपको ही देखता है। मकान मालिक गद्गद होकर प्रसन्न हो जाता है। जिधर देखो, अपना ही रूप देखा। जोर से हँसता है तो उसकी प्रतिध्वनि चारों तरफ गुंजायमान हो जाती है। उसके कान में यह ध्वनि श्री सुनाई पडती है। तो कहता है कि यह मेरी ही आवाज है। मतलब सब ओर मैं ही मैं हूँ।
जिधर देखता हूँ जहाँ देखता हूँ। मैं अपनी ही ताब और शां देखता हूँ।
अभी उसी महल में उसका कुत्ता जाता है तो क्या देखता है कि चारों तरफ हजारों कुत्ते हैं, तो उसकी बुद्धि में ये सब अलग-अलग कुत्ते दिखाई देते हैं। वह अपने से भिन्न उन्हें समझता है। जहाँ उसकी बुद्धि में यह बात आई कि वे सब उससे भिन्न हैं तो उसके मन में राग-द्वेष का भाव जागृत हुआ और लगा मूँकने। उसी के भूकने की प्रतिध्वनि गुंजायमान हो गई। इस प्रकार शब्दों की गाँई (प्रतिध्वनि) से महल भर गया और कुत्ता भँकते-भैंकते मर गया। यह संसार शीशमहल है। अपने स्वरूप से ही राग-द्वेष दृष्टि के कारण, भिन्न- भिन्न देखता है और यह नहीं देखता कि मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। मुझ आत्मा से भिन्न एक भी कण नहीं है। वह अपने स्वरूप को ही भिन्न मानकर पशु बुद्धि के कारण नाना प्रकार के दुःख को प्राप्त होता है। प्यारे ! तू श्वान दृष्टि छोड़ दे। गाँड शब्द के माने ईश्वर है, सब अपना स्वरूप है, वरना डाग, नानात्व (पशु दृष्टि) से स्वयं कष्ट पायेगा। अरे बाप रे! कहाँ मैं मनुष्य, जीव और कहाँ ईश्वर। एकाकी दृष्टि ईश्वर दृष्टि है और नानात्व दृष्टि श्वान दृष्टि है। कम इन दी वर्ल्ड लाइक दी मास्टर जी, ओ, डी-गॉड बट नॉट डी, ओ जी-डॉग।
कहने का मतलब यह है कि सारे विश्व को भगवदृष्टि से देखें, भगवान समझें, जानै-सर्व को एकत्व दृष्टि, आत्म दृष्टि, से जाने। पुराण, उपनिषद्, पिता, भागवत, रामायण सभी तारों से यही आवाज आ रही है। महात्मा प्रह्लाद सात्व दृष्टि बदलने के लिए कह रहे हैं। मृत्यु प्रह्लाद का क्या कर सकेगी, अबांके प्रह्लाद की दृष्टि में मृत्यु भी भगवान है। प्रह्लाद का कुछ न बिगड़ा। स्वरूप आत्मा का ध्यान करते हुए अचल रहा। राणा ने मीरा को हलाहल (ए) पीने को दिया और उसे मीरा पी गई, परन्तु उस विष को पीने से मीरा श्री नहीं हुआ। यह तो साक्षात् गिरधर का ध्यान करके पी गई। कुछ बाल बाँका भी न हुआ। हमें इसका खूब तजुर्बा है। हम पर तो बड़ी-बड़ी मुसीबत आई हैं और रहती हैं। प्रचार कार्य में समय-समय पर बड़ी-बड़ी बाधायें आती हैं, परन्तु कुछ नहीं बिगड़ा। तुम भी परीक्षा करके देखो। यह ब्राह्मी दृष्टि बड़ी सुंदर है। तुम जब अपने आपको भगवान आत्मा जानोगे, अपने 'मैं' का अनुभव करोगे तो तुम्हें 'मैं' ही 'मैं' दिखेगा, नारायण ही नारायण तुम्हें भासेगा।
स एवेदꣲ᳭ सर्वम् - यह सब वही है।
अहमेवेद्ꣲ᳭ सर्वम- यह सब मैं ही हूँ।
आत्मैवेद्ꣲ᳭ सर्वम् - यह सब आत्मा है।
(छ..उ. 7 - 25)
महिर्ष उद्दालक छान्दोग्योपनिषद् में अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझा रहे हैं। आत्मैवेद्ꣲ᳭ सर्वमिति ।
यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञात्ꣲ᳭ स्याद्वाचारम्भणं ।
विकारो नामधेयम् मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।।
(छा.उ. 6-1-4)
जिस प्रकार मिट्टी के बने हुए एक घड़े को जान लेने से मिट्टी के बने हुए समस्त घटादिक पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि ये सब पदार्थ मिट्टी ही है। नाम, रूप तो केवल वाणी का विकार मात्र है। उसी प्रकार अपने स्वरूप आत्मा को जान लो फिर अपने आप का ज्ञान हो जाने से सब ओर अपना ही स्वरूप दिखाई देगा। सारा संसार भगवान दिखाई देगा। व्यवहार तो चल ही रहा है। अभी तक जीव मानकर व्यवहार पालन करते थे और अब भगवान आत्मा जानकर व्यवहार पालन करो।
आये कछु हर्ष नहीं, जाये कछु शोक नहीं ।
बड़े निर्द्वन्द्व हूँ, समझने की बात है ।
देह नेह घेरे नहीं, लक्ष्मी के चेरे नहीं,
सुत वनितादि मेरे नहीं, हरि सो कछु वसात है ।।
लोक की रीति है, मानने की प्रति है,
हार है न जीत है, जाति है न पाति है ।।
निर्भय यही ज्ञान है, सत्य भगवान है,
और कहा ज्ञानी के सींग जम जात है ।।
लोक रीति तो चलती ही रहेगी, चाहे अपने को जीव मानों या ब्रह्मा। जीव मानने से दुःख भोगो और ब्रह्म तो हो ही-आनंद ही आनंद है। यह हर तरफ से सिद्ध है। ज्ञान प्राप्त करने पर ज्ञानी के सींग नहीं जम जाते। तो कहर तरफ से यह है कि प्रह्लाद को किसी तरह से कोई हानि न हुई। प्रह्लाद को मारने की सार्य कोशिशें व्यर्थ गई और प्रह्लाद न मरे। अन्ततोगत्वा जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि यह किसी भी उपाय से नहीं मरता तो एक दिन स्वयं हाथ में खड्ग लेकर क्रोध से लाल हो गरज कर कहता है कि देखता हूँ, अब तेरा ईश्वर कहाँ है? मैं देखूँ कि तू कैसे नहीं मरता। सामने गुरु पुत्र शण्डामर्क खड़े थे, उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि राजन् !
इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्धवा निधेहि भीतो न पलायते यथा ।
बुद्धिश्च पुंसो वयसाऽऽर्यसेवया यावद् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति ।।
(श्रीमद् भा. 7 - 5 - 50 )
अभी इसे एक बार पुनः मेरी पाठशाला में भेज दीजिये। मैं इसके सुधार के लिये भरसक कोशिश करूँगा। आगे यदि यह सुधर जाता है तो ठीक है नहीं तो जैसा कुछ इसका भाग्य होगा, देखा जायेगा। यह छोटा बालक है ऐसा न हो कि डर के मारे कहीं भाग जाये, अतः अभी इसे वरुणपाश में बाँधकर रखे रहो जब तक कि दैत्यकुल के आचार्य हमारे पिता भृगु (श्री शुक्राचार्य जी) न आ जायें। हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को गुरुपुत्र शण्डामार्क को दे दिया और प्रह्लाद फिर पाठशाला में आ गये। अभी तक तो प्रह्लाद स्वयं भगवान में लीन रहते थे, भगवतमय स्थिति में थे, अब पाठशाला के विद्यार्थियों को एकत्र करके उन सबको भी भागवत धर्म का उपदेश करने लगे। स्कूल के विद्यार्थियों में आत्मतत्व का डंका बजाने लगे। वे इस प्रकार संबोधन करने लगे-
कौमार आचरेत्प्राज्ञो धर्मान्भागवतानिह ।
दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् ।।
(7-6-1)
यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् ।
यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत् ।।
(7-6-2)
सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम् ।
सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः ।।
( 7 - 6 - 3)
मेरे साथियों! यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। विद्यार्थियों की सभा एकत्र करके महात्मा प्रह्लाद कह रहे हैं कि हमें जानना चाहिये कि हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य जन्म पाकर हम सबको क्या करना चाहिये? भगवद्धर्म क्या है? और उसका क्या स्वरूप है? समझो भागवत धर्म का मूलभाव-यही समझना है कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सब भगवान है। वे अपने सहपाठी बालकों को 'सर्व को भगवान जानना' ऐसा उपदेश दे रहे हैं। भावगत धर्म सर्वत्र एकत्र भाव की प्रेरणा देता है। मानव शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। हम लोग विषय प्राप्त करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं।
सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम् ।
सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः ।।
(7 - 6 - 3)
यह सब विषय भोग बिना प्रयास के ही प्राप्त हैं, प्रारब्धानुसार ये सब कुछ मिल जाता है। देखते भी हैं कि बड़े-बड़े राजाओं के यहाँ कुत्तों की सेवा में एक नहीं, दो-दो, चार-चार नौकर लगे रहते हैं, जो कि उन्हें स्वच्छ रखते हैं, स्नान कराते हैं, 40-50 हजार की मोटर गाड़ी में बैठाकर कुत्तों को सैर कराने ले जाते हैं-सुंदर सुगंधित साबूनों से नहलाते हैं और महीन मुलायम तौलिये से पोंछते हैं, मखमली गद्दों में सुलाते हैं, सुगंधित इत्र आदि उनके शरीर में लगाते हैं। बताओ, वे कुत्ते कौन-सा साधन किए हैं? यह भी उसका भोग ही तो है और मानव समाज में कोई-कोई रात-दिन मेहनत करके भी अपना पेट नहीं भर पाते। भैया ! तो फिर सुख या दुःख सभी स्वयं प्राप्त हैं-करो या न करो, दुःख हो या सुख जो तुम्हें मिलना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा भोग बिना प्रयास ही सर्वत्र प्राप्त होगा। मनुष्य को 100 वर्ष की अवस्था मिली है। चलो, देखें-उसका बँटवारा करें, 50 वर्ष तो सिर्फ सोना बनाने में व्यतीत हो जाता है। हाँ भाई! सोना क्यों न बनायें-महंगाई जो है।
एक वक्त की बात है। (पू. श्री स्वामी जी अपना अनुभव बता रहे हैं। उस समय आप अवधूत वेश में रहते थे। करीब 1941-42 की बात है।) भ्रमण करते हुए हृषिकेश से पैदल चलकर रात को भीमगोड़ा पहुँचे। वहाँ पर कुछ और साधुओं से भेंट हुई, सत्संग चलने लगा। इस तरह सत्संग में रात्रि के 12 बज गये। हमने साधुओं से कहा कि रात्रि अब अधिक हो गई है, चलो सोना बनायें (भाव था कि चलो विश्राम करें, सोयें)। अब सोना बनाना चाहिये। कुटिया के बाहर गश्ती पुलिस घूम रही थी, उसने सुना कि भीतर साधु लोग सोना बनाने में लगे हैं। उसे शंका हो गई कि यहाँ सोना बनाया जा रहा है। यह सोना बनाने वालों का कोई गिरोह है। वह दौड़कर थाना गया और थानेदार से निवेदन किया कि हुजूर! अमुक कुटिया में साधु सोना बना रहे हैं। थानेदार पिस्तौल, टॉर्च लेकर पुलिस गार्ड के साथ आकर कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया और स्वयं टॉर्च लेकर दरवाजे पर टक टक की आवाज लगाने लगा। दरवाजा खोला गया तो भड़भड़ाकर पुलिस कुटी में घुस आई और टार्च की रोशनी से वे चारों तरफ देखने लगे कि कहाँ पर सोना बनाया जा रहा है? जब देखा तो वहाँ पर सब नंगों से भेंट हुई। एक-एक लंगोट और एक-एक चादर। जब उनसे पूछा गया कि क्या देख रहे हो? तो थानेदार कुछ घबरा गया और कहा कि स्वामीजी ! हम लोगों को पता लगा है कि यहाँ पर सोना बनाया जा रहा है। तो हम लोग जाँच करने आये हैं कि यहाँ पर कोई सोना बनाने वालों का गिरोह ठहरा हुआ है। हम लोग उठकर खड़े हो गए। मैंने कहा भैया ! देख लो और साधुओं से कहा कि चलो शंकर बनो। वे सब इधर-उधर टार्च मारे, फिर वहाँ क्या था, जो उन्हें मिलता। उन्हें बताया कि भाई ! रात्रि अधिक हो गई थी तो हमने साधुओं से कहा कि चलो भाई ! अब सोना बनाया जाए, अब सोना चाहिये। सुनते ही थानेदार बड़ा लज्जित हुआ और कान्स्टेबल को सैकड़ों गालियाँ सुनाता हुआ चला गया। वह कान्स्टेबल कहता रहा कि हुजूर ! हम क्या जानें, बाहर से जो सुना उसका आपको रिपोर्ट दिया। देख लो अब-
गरज यह कि उमर का पचास वर्ष बीत गया सोने (नींद लेने) में, पाँच वर्ष खेलने में, पाँच वर्ष प्रायमरी, छह वर्ष मैट्रिक, तीन वर्ष बी.ए. और दो वर्ष एम.ए. करने में, इस तरह कुल इक्कीस वर्ष निकल गये। अब बच गये कितने ? उन्तीस वर्ष। अब बाबूजी हो गए इक्कीस वर्ष के। श्रीमती जी का पदार्पण हो गया। प्रपंच का बोझ सिर पर लाद दिया गया। भैया ! यहाँ तो सरयूपारी लोग विवाह आठ साल में ही कर देते हैं। बस, आठ वर्ष में ही भौरिया देते हैं और फिर जय सीताराम-
अचीकमद यो न जानाति यो न जानाति बर्बरी ।
अजर्घा यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयताम् ।।
आजकल तो इसमें हरताल लगा दिया गया है, मेंट दिया गया है। क्यों नहीं, यहाँ के समाज को भी तो सुधारना है। हाँ, समय आने पर सुधारने आऊँगा। फिर श्रीमती जी की उपासना के लिए-गहना, द्रव्य आदि-आदि। बहरहाल गीता फैल गई। अब बने बाबा और जब मुण्डी हिलने लगी तब कहते हैं कि यह अवसर अब अध्यात्म जानने का है। जब शरीर बेकाम हो गया, पचपन-साठ वर्ष के हो गए तो फिर भजन करेंगे, ऐसा सोचते हैं। अरे! भगवान को जानना है तो जवानी में जानो, आगे चलकर जीवन आनंदमय बीतेगा। दिल में जब तक जोश है, दिमाग में होश है तभी तक जल्दी से जल्दी आत्मतत्व का ज्ञान सम्पादन करो, प्राप्त करो, समय को मत जाने दो। हाँ-फिर व्याह करो, नौकरी, रोजगार सब कर सकते हो-आनंद से-परन्तु ध्यान रखो, पहिले आत्मतत्व को हासिल करो। शरीर नाशवान है, समय हाथ से मत जाने दो। बूढ़ापे में जर्जर शरीर से अविनाशी अव्यक्त का ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे। प्रभु को, आत्मतत्व को प्राप्त करने के लिए लंगोट कस लो। देखो, हम तो यही अनुभव कराते हैं।
महात्मा प्रह्लाद विद्यार्थियों को अनुभव कराते हैं कि यही भगवत प्रेम है जो हृदय को गद्गद कर आनंद से ओतप्रोत कर देता है। आत्मतत्व को जानने की व्याकुलता के बिना, आत्म तत्व का बोध अर्थात् भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं होती। मन में आत्मा को जानने की अभिलाषा तो करो। इस दरबार में तो प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है और अनुभव कराया ही जा रहा है। शीघ्र अनुभव करो। प्रत्यक्ष, अभी अनुभव करो, इसी जवानी में, बुढ़ापे का इंतजार पत करो-
यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् ।
यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत् ।।
(श्रीमद् भागवत 7-6-2)
महात्मा प्रह्लाद अपने विद्यार्थी बंधुओं को सर्वात्मा भगवान का बोध करा रहे हैं-
न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वयासोऽसुरात्मजाः ।
आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ।।
(श्रीमद् भागवत 7-6-19)
अच्युत् जो भगवान आत्मा हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए बहु आयासः न- अर्थात् कोई अधिक परिश्रम नहीं है। क्योंकि, भगवान सर्व की आत्मा हैं, सर्वत्र हैं, सर्व हैं, सभी में ओतप्रोत हैं और उससे ही सारा चराचर सिद्ध होता है। इसलिए आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहिये, यह थोड़ी सी जिज्ञासा से ही प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि बहुत प्रयास नहीं तो थोड़ा प्रयास होगा। तो आत्म जिज्ञासा होना, भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए यही प्रयास है। अब यहाँ पर कुछ श्रुतियाँ आई हैं-उनका भी स्वागत करें-
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू स्वाम ।।
(कठो. 3-2-24)
अयम् आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः, न मेधया, न बहुना श्रुतेन-जीवन भर प्रवचन सुनते रहो, परन्तु आत्मतत्व का बोध न होगा। न ही बहुत मेधावी (धारणा वाले) को ही इसकी प्राप्ति होती है और न बहुत विद्वान को इसका लाभ होता है। आत्म तत्व को जानने की जब उत्कट जिज्ञासा होती है, मछली के समान जब तड़प पैदा होती है तभी इसकी प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। गत-रात भर नींद नहीं आती, घर-द्वार कुछ भी नहीं सूझता, सिर्फ सनातन ब्रह्म को बानने की प्रबल इच्छा जब होगी तब उसके समक्ष भगवान आत्मा 'मैं' स्वयं प्रगट हो जाता है अर्थात् उसे भगवान आत्मा की अनुभूति हो जाती है।
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ।।
(मुण्डक 3-2-4)
बलहीन पुरुष को आत्मलाभ नहीं होता। यहाँ पर बल का अर्थ शारीरिक बल से नहीं है, वरन इसका अर्थ आत्म जिज्ञासा बल जानना अर्थात् आत्म जिज्ञासाविहीन को आत्म दर्शन नहीं होता। इसका लाभ प्रमादी को नहीं होता। तप से इसकी प्राप्ति नहीं होती। लिंग अर्थात् वेश धारण करने से भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। ' एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम' आत्म जिज्ञासुओं का मुख्य बल, साधन है तो यही आत्म दर्शन की व्याकुलता। चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यासी हो, स्त्री या पुरुष हो आत्म जिज्ञासुओं को जिज्ञासा बल चाहिये। आत्मा को जानने का अधिकार दूसरे को नहीं है। इसका सम्बन्ध मूर्खता, विद्वत्ता से नहीं है। वरन आत्म जिज्ञासा से है। प्रबल आत्मजिज्ञासा जिसको है उसी को आत्म तत्व का बोध होता है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः 11(7 - 6) सर्वभूतानां आत्मत्वात्-भगवान सर्व की आत्मा है, परमात्मा है जो सबका 'मैं' है। आत्मा उसको कहते हैं जिससे सारे चराचर की सिद्धि होती है। इस प्रकार जब महात्मा प्रह्लाद ने अपने सहपाठियों को आत्मतत्व का बोध कराया तो बालक प्रसन्न होकर पूछते हैं कि भैया प्रह्लाद ! यह ज्ञान तुम किसकी कृपा से प्राप्त किये हो? यहाँ तो गुरु महाराज ये सब नहीं बतलाते फिर तुमने कैसे जाना? यदि हम लोगों को बतला सकते हो तो बतलाओ। महात्मा प्रह्लाद कहते हैं- सहपाठियों ! सुनो, जिस समय मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत की कन्दरा में परमेष्ठी ब्रह्माजी का तप करने के लिये गये तो राजधानी को सूना पाकर देवराज इन्द्र, मेरी माता कयाधू का हाथ खींचकर बरबस देवलोक को घसीटकर ले जाने लगा। मेरी माँ कयाधू विलाप कर रही थीं, परन्तु देवराज जबरदस्ती ले जा रहा था। इसी समय रास्ते में देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने इन्द्र को इस तरह की धृष्टता के लिये फटकारा और कहा-देवराज ! यह घृणित कार्य तुम क्यों कर रहे हो? इन्द्र ने कहा-प्रभो! आप जानते ही हैं कि हिरण्यकश्यप कितना घोर तप करने के लिए मन्दराचल पर्वत की कन्दरा में गया है। हिरण्यकश्यप हम लोगों का राज्य छीन लेना चाहता है और यह गर्भस्थ बालक उसका ही वीर्य है। जब यह बालक पैदा होगा तो यह भी अपने पिता के ही समान दुष्ट दैत्य होगा। हम सब लोगों को नष्ट कर देगा। इसीलिये हम कयाधू को ले जा रहे हैं कि जब बालक पैदा होगा तो बालक को मार देंगे और कयाधू को वापस कर देंगे। इस पर देवर्षि नारद कहते हैं-
अयं निष्किल्बिषः साक्षान्महाभागवतो महान् ।
त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली ।।
(7-7-10)
देवराज ! तुम जानते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो-अरे! इसके गर्भ में साक्षात् आत्मनिष्ठ बालक है। यह निष्किल्बिष अर्थात् निष्पाप एवं महान भागवत (भक्त) होगा और भगवान का अनुचर (दास) होगा। इसी की रक्षा हेतु भगवान अवतार लेंगे। यह बालक परम आत्मदर्शी होगा। इस तरह इन्द्र को समाधान करके मेरी माता को नारद जी अपने आश्रम ले आये और कहे कि बेटी ! अब तू यहाँ निर्भयतापूर्वक रह, जब तेरे पति तप करके वापस आ जाएंगे तब तू चली जाना। तेरा अब देवराज कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। तेरा कोई अहित न होगा। तब रानी कयाधू वहाँ रहने को राजी हो गई और प्रार्थना की कि भगवन् ! आप ऐसा करें कि जब तक मेरे पति वापस न आजायें तब तक मेरा यह पावन गर्भ स्तंभित रहे, वह पति के वापस आने के बाद ही पैदा हो। नारदजी ने उसे अभय दिया और कहा- तथास्तु ! बेटी ! तेरी जैसी कामना है, वैसा ही हो। ऐसा कहने के उपरान्त कयाधू नारद जी के आश्रम में रहने लगी। उधर हिरण्यकश्यप ने देवताओं के सौ वर्ष तक घोर तप किया और इतने काल तक मैं अपनी माता के गर्भ में ही रहा। प्रतिदिन देवर्षि नारद मेरी माता कयाधू को भगवत् ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का उपदेश दिया करते थे और वह एकाग्रचित्त होकर प्रेम से सुनती थी। इस प्रकार मैं गर्भ से ही भगवत् भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने लगा। मेरे गुरु भगवान नारद हैं। उनकी ही कृपा से गर्भ में ही मुझे आत्म तत्व भगवद् भक्ति मिली। अभी भी हिन्दू समाज में गर्भिणी को सत्संग करने के लिए कहा जाता है। भगवान की लीला कथा आत्मतत्व का अनुभव गर्भस्थ बालक करता है। गर्भ के बालक पर इसका बड़ा संस्कार पड़ता है। यहाँ भगवान नारद का उपदेश बालक प्रह्लाद ने ग्रहण किया।
आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः ।
अविक्रियः स्वदृग्हेतुर्व्यापकोऽसङ्ग्यनावृतः ।।
(श्रीमद् भागवत 7 - 7 - 19 )
एतैर्द्वादशभिर्विद्वानात्मनो लक्षणैः परैः ।
अहं ममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् ।।
(श्रीमद् भागवत 7 - 7 - 20 )
महात्मा प्रह्लाद कहते हैं - साथियों! सुनो-विचारवान पुरुष को चाहिए कि अपने स्वरूप आत्मा के बारह लक्षणों को भली-भाँति जानकर देहादिकों में जा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मैं-मेरापन है, इस असत्य भाव को त्याग कर मुक्त हो जाए। अपने आप मैं के 12 लक्षण कौन-कौन से हैं? विचार कीजिये-मैं नित्य हूँ, मैं अव्यय अर्थात् पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ अर्थात देहादिक प्रपंच का ज्ञाता हूँ, मैं सर्व का आश्रय (आधार) हूँ, मैं अक्रिय हूँ, मैं अपने आप स्वयं का दृष्टा हूँ, मैं सर्व का कारण हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं असंग हूँ, निर्लेप हुँ मैं अनावृत-आवरण (अज्ञान रहित) हूँ। इन्हीं 12 लक्षणों को अपने स्वरूप आत्मा 'मैं' में जानकर सुमेरु पर्वत के समान अचल हो जाना चाहिये। मैं आत्मा के जान लेने पर मैं-मेरा, तू-तेरा इस अज्ञान का नाश हो जाता है। मैं- मेरा पन यह असत्य भाव अज्ञान से पैदा हुआ है, इसलिए इस अज्ञान को त्यागकर अपने आप मैं आत्मा को जानना चाहिये। विचारवान मनुष्य के लिए यही ज्ञातव्य है।
स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् ।
क्षेत्रेषु देहेषु तथाऽऽत्मयोगैरध्यात्मविदब्रह्मगतिं लभेत ।।
(श्रीमद् भागवत 7-7-21)
जिस प्रकार खोट भाग को अलग करके हेमकार (स्वर्णकार) खरा भाग को ग्रहण कर लेता है। इस तरह जिन-जिन पदार्थों को तू मेरा कहता है वह खोट है, उनको छोड़कर शुद्ध भाग 'मैं' आत्मा को ग्रहण कर लेना चाहिये। शुद्ध भाग 'मैं' का 'मैं' ही खरा हूँ।
बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः ।
ता येनैवाननुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः ।।
(7 - 7 - 25)
इस प्रकार से प्रह्लाद ने अपने सहपाठियों को उपदेश दिया। इस उपदेश को ग्रहण कर सभी सहपाठी प्रह्लाद हो गये। सबकी धारणा आत्मतत्व से ओतप्रोत हो गई। सभी वही राग आलापने लगे। गुरुजी शण्डामर्क बालकों की ऐसी बुद्धि देखकर घबरा गये। अब गुरुजी क्या करें? प्रह्लाद पर बहुत बिगड़े कि तुमने सहपाठियों को भी बिगाड़ दिया, अब तुम्हें नहीं पढ़ाया जायेगा। इस तरह पाठशाला से निकालकर उसे पकड़कर राजा हिरण्यकश्यप के पास ले जाकर कह दिया कि यह बालक स्वयं तो बिगड़ा हुआ है, ऊपर से पाठशाला के अन्य बालकों को भी इसने भड़का दिया है। अब आप ही जाने कि इसे क्या किया जाय। इस पर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो, लाल-लाल आँखें करके प्रह्लाद को फटकारता है।
श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुःसहं तनयानयम् ।
कोपावेशचलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दधे ।।
(7-8-3)
हे दुर्विनीत मन्दात्मन्कुलभेदकराधम ।
स्तब्धं मच्छासनोद्भूतं नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम् ।।
(7-8-6)
क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः ।
तस्य मेऽभीतवन्मूढ शासनं किंबलोऽत्यगाः ।।
(7-8-7)
अरे मूर्ख प्रह्लाद ! क्या तू जानता नहीं कि जब मैं तनिक-सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोकों के सब लोकपाल काँप उठते हैं। फिर मूर्ख तू किसके बलबूते पर निडर होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहा है। क्या तू जानता नहीं कि मेरे क्रोध से तीनों लोक कंपायमान हो जाते है। लोक लोकान्तर का तेज जाता रहता है और तू इतना निर्भय है। तस्य मेऽभीतवन्मूढ शासनं किंबलोऽत्यगाः ।। (7 - 8 - 7) तू किसके बल से इतना निर्भय है? तू तो कहता है कि तेरा जगदीश व्यापक है, चारों तरफ है, संसार में ओतप्रोत है। तो मैं पूछता हूँ कि वह अब कहाँ है? देख, तू अभी शीघ्र ही मेरे हाथ से यमलोक जायेगा, तू यमराज का पाहुना होने जा रहा है। तेरा जगदीश व्यापक है तो-
यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः ।
क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात्स्तम्भे न दृश्यते ।।
(7 - 8 - 13)
मन्दभागिन ! तू जो मेरे अतिरिक्त किसी और को जगत का स्वामी कहता है तो देखूँ तो तेरा जगदीश्वर कहाँ है? यदि तेरा जगदीश सर्वत्र है, यदि वह सर्व है, सर्व ओर है तो फिर है कहाँ? इस खंभे में मैं उसको क्यों नहीं देख रहा हूँ देखता हूँ वह तुझे कैसे शरण देता है? वह सब है तो दिखाई क्यों नहीं देता। क्या मैं तुझे नहीं देख रहा हूँ? अच्छा, अब तू मेरे हाथ से मारा जायेगा या फिर तेरा रक्षक आकर मुझे मारेगा। समझो हिरण्यकश्यप आस्तिक था। यदि आस्तिक न होता तो वह ब्रह्माजी का तप करने कैसे जाता? यह भगवान विष्णु का विरोधी था। तेरा जगदीश सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा तुझे इस खंभे में भी दिखाई देता है? वह दैत्य क्रोध के कारण आपे से बाहर हो गया और जोर से एक मुक्का खंभे को मारा। खम्भा टूट गया और महाभयंकर शब्द हुआ। भगवान का श्री नृसिंहावतार हुआ। भगवान विचित्र रूप में प्रकट हुए। ऊपर का भाग तो सिंह का था और नीचे का भाग नर (मनुष्य) का। दूसरे दैत्य, भगवान के इस विकराल रूप को देखकर भाग खड़े हुए। सिर्फ हिरण्यकश्यप, नृसिंह और प्रह्लाद रह गये। उस समय हिरण्यकश्यप भगवान नृसिंह विग्रह को देखकर हाथ में खड्ग लेकर दौड़ा तो प्रभु ने दौड़कर उसे दबोच लिया। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप से कहा कि देख तूने कभी ऐसा रूप ब्रह्माजी की सृष्टि में देखा है? कभी ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि की है? बुढ़उ (ब्रह्मा) का वचन भी तो भगवान को सत्य करना था। न मेरे पास कोई अस्त्र- शस्त्र है। यहाँ नख ही शस्त्र है। देख ले, मेरे पास कोई आयुध नहीं है। उसे गोद में लिटाकर ड्योढ़ी के बीच में उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। 'मैं' से 'मैं' का मेल हो गया। हिरण्यकश्यप का कलेवर तेज प्रभु में लीन हो गया। इस विकराल विचित्र रूप को देखकर देवता लोग भी घबरा गये। भयानक स्वांग को देखकर पास में जाने की हिम्मत देवताओं की भी नहीं हुई। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। जब ब्रह्माजी भी पास न जा सके तो सभी देवताओं ने महारानी लक्ष्मीजी को आग्रह किया कि माता ! तुम्हीं जाकर प्रभु का क्रोध शांत करो। लक्ष्मीजी प्रभु के पास तक तो गई, परन्तु उनका विकराल रूप देखकर वह भी डर गई और वापस लौट पड़ीं। बुढ़ठ (ब्रह्मा) महाराज कहते हैं- माता ! जाओ, प्रभु का क्रोध शांत करो। लक्ष्मी जी कहती हैं कि जिस रूप की मैं सेवा करती हूँ वह तो भुवन सुंदर है। यहाँ पर तो भगवान भयावह रूप धारण किये हैं। लक्ष्मी जी भी पास न जा सकीं। प्रभु का क्रोध शांत न हुआ, तो ब्रह्माजी ने प्रह्लाद से कहा बेटा । भक्तवत्सल भगवान तेरे लिए ही आये हैं तू ही जाकर शांत कर। प्रह्लाद जाकर श्री-चरणों में लिपट गये। भगवान प्रसन्न होकर भक्त प्रह्लाद को गले से लगा लिये और कहे कि बेटा। वरं वृणीष्व-तुम प्रसन्नचित्त से वर मांगो-
प्रह्लाद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम ।
वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम् ।।
( श्रीमद् भागवत 7-9-52)
तो महात्मा प्रह्लाद कहते हैं- भगवन्! मेरे पिता का भी कल्याण हो जाये क्योंकि वह आपका तथा आपके भक्तों का निंदक, द्वैषी एवं उन्हें कष्ट पहुँचाने वाला था। तो भगवान नृसिंह कहते हैं कि बेटा !
त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ
यत्साधोऽस्य गृहे जातो भवान्वै कुलपावनः ।।
(7-10-18)
क्या अभी तक तुझे अपने पिता के उद्धार में शंका बनी हुई है? जबकि मेरे करकमलों द्वारा उसका वध हुआ है और फिर जिस कुल में तेरे समान एक आत्मदर्शी भक्त जन्म ले लेता है उसके इक्कीस पीढ़ी आगे और पीछे के पितर तर जाते हैं। वह कुल पवित्र हो जाता है। जननी जो माता है उसका कोख शुद्ध हो जाता है। वसुन्धरा जो पृथ्वी है वह ऐसे आत्मनैष्ठिक को पाकर पुण्य रूप हो जाती है। इसलिए तेरे विमल कुल में अब कोई पापिष्ट न होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे कुल में अब किसी का भी वध न करूँगा। क्योंकि, तेरा कुल अब नारायण कुल, भगवद् भक्तों का कुल हो गया। महात्मा प्रह्लाद की कुल परम्परा महर्षि कश्यप से शुरु होती है। महर्षि कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष । हिरण्यकश्यप के प्रह्लाद-उनके पुत्र हुए विरोचन-राजा विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि और उसके पुत्र हुए राजा वाणासुर। तब से महात्मा प्रह्लाद के कुल में प्रभु द्वारा कोई वध नहीं हुआ, क्योंकि नृसिंहावतार में भगवान प्रतिज्ञा कर चुके थे कि इस कुल में अब मैं किसी का भी वध नहीं करूँगा। दहालांकि कृष्णावतार में उषा-अनिरुद्ध के संबंध में भगवान और वाणासुर का युद्ध हुआ था, परन्तु भगवान ने उसका वध न कर उसके मान का मर्दन किया था। इसके बाद प्रभु ने फिर प्रह्लाद को आज्ञा दी कि तुम अपने दैत्य कुल की परम्परा के अनुसार अपने पिता का मृतक कर्म सम्पादन करो और फिर राज्याभिषेक कराकर पृथ्वी का पालन करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर भक्त प्रह्लाद कृतकृत्य हो गया। इतना कहकर भगवान प्रह्लाद को आशीर्वाद देकर अन्तर्धान हो गये।
---------------
चतुर्थ दिवस
गजेन्द्रोपाख्यान के माध्यम से अस्तित्व निरुपण श्री कृष्ण जन्मकथा
21-2-1969, प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
अनन्त नाम रूपों में अभिव्यक्त, अहमत्वेन प्रस्तुरित, महामहिम, स्वात्मस्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित आत्मजिज्ञासुगण !
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।।
अनादिकाल से अज्ञान की घोर निद्रा में सोने वालों भव्य जीवों ! उत्तिष्ठत- उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो, किसी श्रेष्ठ महापुरुष के उपसन्न होकर अपना आत्म कल्याण करो। यहाँ पर अध्यात्म निरूपण श्रीमद्भागवत परमहंस संहिता के आधार पर हो रहा है। कल का प्रसंग प्रह्लादोपाख्यान था। आज गजेन्द्र मोक्ष (गजेन्द्रोपाख्यान) श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कन्ध के माध्यम से अध्यात्म निरूपण होगा।
आसीद्गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः ।
क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्योजनायुतमुच्छ्रितः ।।
(8 - 2 - 1)
क्षीरसागर से घिरा हुआ चित्रकूट नाम का एक महाविशाल पर्वत था। पर्वत नाना प्रकार के वृक्ष, लताओं एवं बेलियों से ढँका हुआ था। कूट अर्थात् धातु। वह त्रिकूट पर्वत माला स्वर्ण, चांदी एवं तांबा, इन धातुओं से परिपूर्ण थी। उस पर भगवान वरुणदेव का एक विशाल उद्यान था। उसमें सुंदर-सुंदर रमणीक स्थान, खेलकूद, आमोद-प्रमोद एवं आखेट के अनेक स्थल थे। यह प्रसंग गजेन्द्र मोक्ष का आख्यान्, अध्यात्म तत्व से भरपूर है। ध्यान से इसका मनन करना। उद्यान में एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में नाना प्रकार के मनोरम कमल खिले थे। उस सरोवर में गजेन्द्र अपनी हथिनियों को साथ लेकर स्नान एवं जलक्रीडा के लिए प्रवेश किया वह सरोवर में खूब आनंद से स्नान कर, जल पी, शांत होकर अपने हथिनियों एवं बच्चों के साथ जल क्रीडा करने लगा। उस सरोवर में एक बहुत बड़ा मगर भी था। वह महादुष्ट ग्राह पूर्वजन्म में हू-हू नाम का गंधर्व था और देवल ऋषि के शापवश ग्राह हो गया था। उसने जल के भीतर ही गजेन्द्र का चरण पकड़ लिया और जल की ओर खींचकर ले जाने लगा। गजेन्द्र को संकट में देखकर पहिले तो हथिनियों ने बल लगाकर गजेन्द्र को बाहर निकालने की कोशिश की, परन्तु ग्राह बड़ा बलवान था, देव गजेच्या सारी शक्ति लगाने पर भी गजेन्द्र को ग्राह के चंगुल से न छुड़ा सकी तो चिंघाड़ मार-मारकर भाग गईं। अब गजेन्द्र अकेला पड़ गया। गजेन्द्र भी शापित था। वह पूर्वजन्म में राजा इन्द्रद्युम्न था जिसने महर्षि अगस्त के शाप से गज (पशु) योनि में जन्म लिया था। वह गजेन्द्र भी काफी बलशाली था। गज और ग्राह एक हजार वर्ष तक घोर संग्राम करते रहे। कभी गजेन्द्र ग्राह को असीटकर बाहर लाता औरकभी ग्राह गजेन्द्र को घसीटकर पानी में ले जाता। इस तरह एक हजार वर्ष तक दोनों लड़ते रहे। अन्ततोगत्वा गजेन्द्र थक गया। जब उसका सारा बल नष्ट हो गया तो उसने अपने पूर्वजन्म के संस्कार के कारण एक कमल पुष्प को सूँड़ से उठाकर अनन्त भगवान के शरण गया। आत्मजिज्ञासुओं ! जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि जब तक उसके पास किसी प्रकार बल रहता है, बुद्धिबल, नीति बल, विद्या बल, जन बल, धन बल कुछ भी रहता है तब तक वह भगवान की शरण नहीं होता। भगवान की शरण में तभी जाता है जब वह निराधार, निराश्रय हो जाता है। अन्ततोगत्वा जब गजेन्द्र अपने को निर्बल निराश्रय पाया तो भगवान नारायण की शरण में गया और भगवान की स्तुति करने लगा। यह गजेन्द्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत का आठवाँ स्कन्ध है। इस स्कन्ध में अनन्त 'अस्तित्व' का निरूपण है। आत्मतत्व का 'अस्तित्व' का प्रतिपादन हो रहा है। जो जहाँ बैठे हो, आनंद लो। गजेन्द्र सूँड़ में पुष्प लेकर भगवान की स्तुति करता है।
ॐनमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्कम् ।
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ।।
(श्रीमद् भागवत 8-3-2) देखो, इस श्लोक में प्रणव और पल्लव दोनों हैं। जहाँ जिस श्लोक में प्रणव और पल्लव दोनों लगा हो वह फिर श्लोक नहीं वरन् मन्त्र कहलाता है। यहाँ ॐ प्रणव एवं नमः पल्लव है। इस गजेन्द्र स्तुति में जितने भी श्लोक हैं वे सब मंत्र हैं। महान संकट से संकट क्यों न हो इन मंत्रों के पाठ, स्मरण में संकट तत्काल मिट जाता है। आपत्तियों में इसका जप करने से दुःख का नाश होता है। ये मंत्र आपत्ति नाशक हैं।
ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्कम् ।
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ।।
(8 - 3 - 2)
इस मंत्र में 'धीमहि' क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी तरह गायत्री मंत्र में भी 'धीमहि' का प्रयोग हुआ है।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरिण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात् ।।
'धीमहि' यह क्रिया है-हम इनका ध्यान करते हैं।
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् ।
योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् ।।
(श्रीमद् भागवत 8-3-3)
एतद् चिदात्मकम् यत् तस्मै भगवते नमः यह जो चैतन्य धनभूत आत्मा अव्यक्त भगवान हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। जिज्ञासुओं ! एतद् किसके लिए आता है? एतद् चिदात्मकम्-यह जो चैतन्य तत्व भगवान हैं उसको मेरा नमस्कार है। देखो यह जो भास है-विकल्प का एकदम अभाव कर दो। 'यह क्या है' ऐसा विकल्प मत करो। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो विकल्प का निर्मूल अभाव कर दो। पहिले सूत्र नोट कर लो फिर व्याख्या करेंगे- 'विकल्पाभाव भगवान। विकल्पाभाव भगवान। विकल्पाभाव भगवान।'
जगत भाव (विकल्प) के अभाव में आधिभौतिक भगवान।
नर विकल्प के अभाव में-आधिदैविक भगवान।
जीव विकल्प के अभाव में आध्यात्मिक भगवान।
( पू. श्री स्वामी ताली बजाकर समझा रहे हैं।)
देखों - यह शब्द विकल्प है। पहिले दिन के प्रवचन में तुम्हें विकल्प क्या है? इसका अनुभव कराये थे। 'शब्द ज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ।' अर्थात् शब्दका तो ज्ञान हो, परन्तु वस्तु का अभाव हो उसे विकल्प कहते हैं। भास पर जगत का जो विकल्प, इस विकल्प को हटा दो, तो फिर यह भगवान का आधिभौतिक स्वरूप है। भगवान राम कृष्णादि का जो लीला विग्रह रूप, यह भागवान का आधिदैविक स्वरूप है और जो 'मैं' नाम से प्रस्फुरित प्रस्फुटित एवं अभिव्यक्त हो रहा है वह भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है। भगवान के आधिदैविक स्वरूप को नर मानना महामोह है और स्वस्वरूप भगवान आत्या 'मैं' आध्यात्मिक स्वरूप को जीव मानना सम्मोह है। रामायण में गरुड़ को महामोह हुआ था।
महामोह उपजा उर तोरे। वेगि न मिटइ कहे खग मोरे ।।
महारानी सती को भगवान राम में नर का भ्रम हुआ था। महात्मा भुशुण्डि को भगवान राम में नर का भ्रम हुआ था। ब्रह्माजी को भगवान श्रीकृष्ण में ना का भ्रम हुआ था। इन सब विकल्पों (भावनाओं) को महामोह जानो। अपने मैं आत्मा में जीव की भावना कि मैं जीव हूँ, इसे कहते हैं संमोह।
भैया ! यह जो भास है वह भगवान ही है। अब इस पर जगत का विकल्प करते हो कि यह संसार है तो यही मोह है, माया है। लकड़ी में डंडा, मेज, कुर्सी, पलंग, चौखट आदि की कल्पना करना यही विकल्प है। अरे, लकड़ी तो लकड़ी ही है। डंडे का विकल्प हटा लो तो लकड़ी ही लकड़ी है। आभूषण का विकल्प सोने से हटा दो। वस्त्र का विकल्प धागे से हटा दो। घटादि का विकल्प मिट्टी से हटा दो। इसी प्रकार भगवान भास पर जो जगत का विकल्प कर रहे हो कि यह संसार है इस विकल्प को हटा दो। भगवान आत्मा 'मैं' पर से जीव का विकल्प हटा दो, तो फिर सब भगवान ही हैं।
ॐनमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्कम् ।
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ।।
यह जो चैतन्य स्वरूप नारायण है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। जी हाँ- अब इस भास में ही ग्राह और गजेन्द्र दोनों हैं। एक विकल्प ग्राह है और दूसरा विकल्प गजेन्द्र है। जब यह (भास) भगवान है तो इन दोनों विकल्पों का भी अभाव हो गया और भगवान ही भगवान शेष रह गया। ये बात है-देखो, समझो विषय, विकल्पाभाव अर्थात् विकल्प के अभाव में, विकल्प चाहे आधिभौतिक पर हो, आधिदैविक पर हो या आध्यात्मिक पर हो, इन विकल्पों का अस्तित्व न रहा कि यह संसार है, नर है या जीव है।
भगवान शंकर और महारानी सती आ रहे थे तो मार्ग में ही भगवान राम को तपस्वी रूप में देखकर भगवान शंकर कहते हैं-
जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले मनोज नसावन ।।
बाबा और बबाइन - बाबा कहते हैं- जय सच्चिदानंद और बबाइन पड़ गई चक्कर में। भगवान आधिदैविक भी हो नहीं रहा। भगवान शंकर ने भगवान राम को जैसा देखा वैसा ही नमस्कार किया। गरज यह कि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक यह भी विकल्प ही है। जब इन तीनों विकल्पों का अभाव हो गया तो रह गया 'मैं'। अवाङ्गमनसगोचर चिन्मय भगवान आत्मा ही आत्मा रह गया। यही तूष्णी पद है। भास पर से जगत का विकल्प हटा दो तो विकल्प के अभाव में सूत्र लिखो-जगत के विकल्प भाव में तीनों विकल्प निहित हैं। जब तक विषय को पूर्णरूपेण नहीं समझाया जाएगा तब तक समझ में न आएगा। हाँ-तो, जगत के विकल्प भाव में तीनों विकल्प निहित हैं। जगत के विकल्प भाव में स्रष्टा, भर्ता, हर्ता, ये तीनों विकल्प निहित हैं। जगत विकल्पाभाव में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सारे चराचर के विकल्प का अभाव हो गया और श्रोता एवं वक्ता विकल्प का भी अभाव हो गया। तो समझो-क्या कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है? यही चिन्मय पद है। माया का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। मार दो छलांग इस दरिया में बह जाओ, इस दरिया का कोई ओर छोर नहीं-न इसका इब्तिदा है, न इन्तिहा है, न दरम्यान है अर्थात न आदि है, न अन्त है न मध्य है। अब बोलो-किससे आँखें बंद करोगे? जिससे आँखें बंद करते हो क्या वह वस्तुतः है? जिससे कान बंद करते हो रूई ढूँस-दूँस कर कि शब्द न सुनाई पड़े, बस ! क्या वह है? जिस मन को रोकना चाहते हो, क्या वह मन है? बस, हो गया बस गये सारे विकल्प, रह गया 'अस्तित्व'। अब कहाँ बाहर और कहाँ भीतर, बाहर भीतर भी तो शरीर की ही अपेक्षा से है। जब शरीर विकल्प का ही अभाव हो गया तो कहाँ बाहर और कहाँ भीतर। ' एतच्चिदात्मकं यत तस्मै भगवते नमः ।' शिव भैया ! भगवान भास पर जगत का विकल्प हुआ। जब जगत का विकल्प हुआ कि यह संसार है तब चार विकल्प पैदा हो गये-देश, काल, वस्तु और कर्ता। अच्छा ! यह संसार है, तो इसको किसी न किसी ने बनाया भी होगा। सबसे पहले सृष्टिकर्ता (ब्रह्मा) का विकल्प हुआ। फिर इसका पालन कौन करता है? तो पालक विष्णु का विकल्प हुआ। फिर संहार कौन करता है? संहार के विकल्प से शंकर का विकल्प हुआ और फिर इसी विकल्प पर ही छहों दर्शन बन गये। कम से कम दर्शनाचार्यों को यह सोचना था कि जिसकी हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वास्तव में क्या वह है?
विद्वजनों ! ध्यान से सुनो, भगवान को संसार मानकर, इस संसार विकल्प मात्र पर ही छहों दर्शनों की प्रतिष्ठा है। न्याय कहता है कि इस संसार का कोई न कोई बनाने वाला (कर्ता) है। न्याय मानता है कि इस संसार का निमित्त कारण भगवान, उपादान कारण प्रकृति और साधारण कारण जीव है। जैसे घट का निमित्त कारण कुम्हार, उपादन कारण मिट्टी और साधारण कारण जिसके लिए बना। इसी को न्याय का कर्तावाद कहते हैं। निमित्त कारण ईश्वर ने, उपदान कारण प्रकृति को लेकर साधारण कारण जीवों के शुभाशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए जगत का निर्माण किया। यह न्याय का सिद्धांत है। तो धन्यहै इस विकल्प को कि इसने बड़े-बड़े दर्शनाचार्यों को भी नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा।
सांख्य कहता है कि न्याय का कहना गलत है। संसार प्रकृति का परिणाम है। जैसे दूध बिगड़कर दही बन जाता है, इस तरह प्रकृति विकृत होकर संसार के रूप में दिखाई दे रही है। यह परिणामवाद है। प्रकृति और पुरुष के योग का परिणाम जगत है। दो भिन्न पदार्थ मिलकर तीसरे का निर्माण करते हैं। मीमांसा का कर्मवाद है। वैशेषिक का कालवाद है, वेदान्तियों का विवर्तवाद है। जिस प्रकार रज्जु का विवर्त सर्प है, इसी प्रकार ब्रह्म का विवर्त जगत है। 'अब तो फुरफुरी आ गई है।' सर्वसाधारण के लिए वेदांत विषय सरल करके बता रहे हैं। मालपुआ गरम-गरम खाना हो तो खाओ, नहीं तो गन्ना, गेहूँ जिंदगी भर बोते रहो, तुम जानो। भाई ! इसलिए जिसका दर्शन है उस वस्तु का प्रतिपादन करते हैं कि विकल्प का? पोल खुल गई। अरे! जगत ही नहीं तो कर्ता, भर्ता, हर्ता का विकल्प ही कहाँ? रह गया भगवान का भगवान। वाह-
ॐनमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्कम् ।
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ।।
अब प्रश्न करो- यह (भास) जो देख रहे हो, क्या यही भगवान है? पहिले देखना सिद्ध करो तब बतायें। पहिले तुम देखना सिद्ध करो। डंडे का विकल्प हटा दो। विकल्प दृष्टिगम्य है या विकल्पक दृष्टिगम्य है? विकल्प दृष्टिगम्य है। विकल्पक अर्थात जो विकल्प करता है। विकल्प जो किया जाता है।
अच्छा, समझना विषय- प्रपंच कहो या संसार, एक ही मतलब है। अनुभव करो (ताली पीटकर बतलाते हैं) शब्द- यह शब्द विषय है, तो कर्ण इन्द्रिय कब बनी? जब विकल्प करते हो कि यह शब्द विषय है, ऐसा मानोगे तब शब्द विषय है, नहीं तो भास ही भास रहेगा। जब विकल्प करोगे तब विषय पैदा होगा और तभी उसी वक्त उसे ग्रहण करने के लिए कर्ण इन्द्रिय पैदा होगी। इन्द्रिय पैदा होगी। ग्राह्य और ग्राहक एक ही काल में पैदा होते हैं। छोटा बालक दो-चार महीने का वह भी सुनता है, परन्तु क्या उसके हृदय में विकल्प मात्र ही रह जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वह शब्द विषयको ग्रहण न करेगा। बालक के सामने काला नाग भी रख दो तो उसे वह खिलौना जान मुँह में ले जाएगा, क्योंकि उसमें सर्प का विकल्प (भाव) ही नहीं है तो बच्चे की दृष्टि में वह भास है। वाह ! तुम्हारे अंदर विकल्प है कि यह सर्प है-काट खायेगा, वह काट न ले, डस न ले। इसलिये तुम्हें भय लगता है। जितनी उपाधि है, विकल्प भाव में है। विकल्पाभाव में तो जितने विकल्प हैं वे भास ही हैं।
जीव कहो या माया-जीव, प्रपंच इत्यादि विकल्पों का आधार विषय 'मैं' भगवान आत्मा सच्चिदानंद घनभूत के कौन होगा? तो विकल्पाभाव शुद्ध तत्व रह गया। विकल्प एवं विकल्पक (जो विकल्प करे) सब लुप्त हो गये। अब प्रश्न होता है कि जो विकल्पक है वह चैतन्य है-अस्तित्वान है अथवा अस्तित्वहीन? यदि कहो कि विकल्पक अस्तित्वहीन नहीं वरन् अस्तित्ववान है-चेतन है-तो फिर उसे क्या मुसीबत पड़ी है कि अपने आपको कुछ माने ? जीव, प्रपंच, तीनों अध्यास, सत, रज, तम, तीनों गुण, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चतुष्ट अन्तःकरण, पंच विषय आदि क्योंकि यह आप्तकाम है। क्यों माने? किसको माने? श्रीमान जी ! जो विकल्प है वह निर्विकल्प है या सविकल्प ? यदि कहो कि विकल्प निर्विकल्प है तो निर्विकल्प से विकल्प कैसे होगा और यदि कहो कि विकल्प सविकल्प है, तो विकल्प हमेशा अस्तित्वहीन होता है, इसलिये जो है ही नहीं वह विकल्प क्या करेगा? अर्थात् विकल्प न तो निर्विकल्प से हुआ और न सविकल्प से, विकल्प तीन काल में हुआ ही नहीं। यह बात है भैया! यही अध्यात्म है। केवल अस्तित्व आत्म तत्व 'मैं' का 'मैं' रह गया। विकल्प हुआ ही नहीं। इसलिए एतच्चिदात्मकर्क यत तस्मै भगवते नमः। यह जो चैतन्य भगवान है, उसको नमस्कार है।
ॐनमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्कम् ।
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ।।
अच्छा, इसका भाव लग गया न। अब आगे चलो। अब यह सवाल है कि गजेन्द्र ने इसको चैतन्य क्यों कहा? अच्छा, सुनो-
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् ।
योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् ।।
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् जो यह है, जिसमें यह है, जिससे यह है, जिस करके यह है, और जो स्वयं ही यह है, जो इससे और इससे परे है वह स्वयंभू भगवान सच्चिदानंद की मैं शरण हूँ। यह कितना सुंदर मंत्र है। कैसा विलक्षण भाव है इसका। कभी कोई हिंसात्मक जानवर सामने आ जाये- हिंसात्मक जीव-अरे भाई। चाहे मनुष्य ही क्यों न हो-जब मारने आया है तो वह हिंसात्मक जीव ही माना जायेगा। हाँ, यह भाव विकल्प भाव है, विकल्प भाव में वह शत्रु है और विकल्पाभाव में 'मैं' ही हूँ। निकाल दो विकल्प को। फिर मैं शत्रु हूँ-यह शत्रु है यह भाव न रहेगा। तम् स्वयंभुवम् आत्मानं अहं प्रपद्ये (शरण्ये) उस स्वयंभू भगवान की मैं शरण हूँ। स्वयंभू का मतलब होता है जो पैदा न हुआ हो। जो पैदा हो उसका नाम स्वयंभू नहीं होगा। अरे ! व्यापक सच्चिदानंद समझो। जो स्वयं हो-उसको स्वयंभू । सत्तापद का प्रतिपादन है। यह सत्तापद है। देखो - व्याकरण शास्त्र में सिद्धांत कौमुदी के अंदर सबसे पहिली धातु-भू-सत्तायाम् है। यहाँ भू-धातू का सत्ता ही अर्थ क्यों किया गया? पाठशाला में, बचपन में, जब गुरुजी से पढ़ते थे तो यह धातु पढ़ी थी। सत्ता परब्रह्म का वाचक है।' सत्तार्थ निर्देशोपेयम् सत्याख्यस्य परब्रह्म स्मरणात् इति महाभाष्यम्।' सत्ता शब्द से परब्रह्म का स्मरण होता है इसलिए परम मांगलिक समझकर भू-धातू का अर्थ सत्ता ही किया गया है। तम् स्वयंभुवम् (अस्तित्वं) अहं प्रपद्ये-अर्थात् उस स्वयंभू भगवान आत्मा की मैं शरण हूँ।
जिस लकड़ी में डंडा, जिस लकडी से डंडा, जिस लकड़ी करके डंडा और जो लकड़ी स्वयं ही डंडा है। इसी प्रकार जिसमें यह, जिससे यह, जिस करके यह और जो स्वयं ही यह। अब आ गया समझ में तुमको ? 'डंडा है'- देखो, बुद्धि से न समझो यह बुद्धि का विषय नहीं है। यहाँ भगवान आत्मा का प्रतिपादन हो रहा है। इसलिए इसे 'मैं' आत्मा ही समझेगा, बुद्धि बेचाया का समझेगी, जबकि वह बुद्धि का विषय ही नहीं है। वहाँ तक बुद्धि की गम नहीं है।' उंडा है'- यह लकड़ी करके सिद्ध हो रहा है कि डंडा करके? लकड़ी करके सिद्ध हो रहा है। इसमें से लकड़ी निकाल लो और यदि डंडा रहे, तभी डंडे का अस्तित्व सिद्ध होगा। परन्तु ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो डंडा चला गया, रही लकड़ी। अब 'लकड़ी है' तो लकड़ी का जो 'है' है वह 'है' है कि लकड़ी है? जिस पर उसका अस्तित्व है अर्थात् पृथ्वी, क्योंकि लकड़ी पार्थिव भाग है। पृथ्वी करके ही लकड़ी सिद्ध होती है, तो लकड़ी गई। अच्छा ' पृथ्वी है' तो पृथ्वी का कारण जल है इसलिए पृथ्वी भी गई। चलो 'जल है' तो जल में जो 'है' पना है वह जल का है कि उसके कारण अग्नि का है? अग्नि का है। तो जल भी गया। अच्छा 'अग्नि है' तो अग्नि में जो 'है' है वह अग्नि का कारण वायु है। तो अग्नि भी गई। अच्छा, फिर देखो 'वायु है'-वायु में जो 'है' है वह वायु का कारण आकाश है। जो 'है' आकाश का है, वही है सारे चराचर का है और जो 'है' सारे चराचर का है, वही आकाश का भी है। यहाँ 'है' अस्तित्व का बोधक है। यहाँ कर्तापद भी है और क्रिया पद भी है। जो 'है' आकाश का है उसी का नाम तो आकाश है।
अब आ जाओ फिर विषय पर जिसमें यह है, जिस करके यह है और जो स्वयं ही यह है, उस अस्तित्व, चिन्मय परिपूर्ण, व्यापक भगवान की मैं शरण में हूँ। (पू. श्री स्वामी जी 'मुक्तोद्गार पुस्तक' से आकाश समीक्षा लेख निकालकर एक सेवक से पढ़ने को कहते हैं। निकालो आकाश समीक्षा लेख पढ़ा जा रहा है और पू. श्री स्वामीजी भाव बता रहे हैं-
-आकाश समीक्षा -
काश! आकाश आकाश होता, तब तो आकाश आकाश ही होता। काश ! आकाश आकाश ही होता, तब आकाश को तिरोहित कौन करता?
आकाश तीखे स्वर में बोला- 'मैं आकाश महान न होता तो समस्त चराचर को अवकाश कौन देता।'
आकाश झाडी में मुस्कराकर बोला- 'ऐ हमनाम ! तू काश चराचर का अवकाश है तो मुझ आकाश का कौन अवकाश है? काश! तू स्वतः, स्वतः सिद्ध है तब आकाश ही है। काश! तू परतः सिद्ध है तब तू है ही नहीं।'
आकाश दबे स्वर में बोला- काश! मैं आकाश न होता तो मुझ आकाश को छुपाने का अवकाश कौन देता? मुझ आकाश के अवकाश मंदिर में ही तो तुझे आँख मिचौली खेलने की जगह मिली है। मैं कैसा अनोखा मंदिर हूँ। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी कितने सुंदर चारों स्तम्भ हैं। पंच महाभूत कितना उच्च वैकल्पिक शिखर है। ऐसे अभाव रूप मंदिर में तू आकाश का आकाश, यानी मैं का मैं ही, जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों ही प्रसरित है। अमुक रूप कैसा बेमिसाल घूंघट है। ऐ परदानशी, परदा उठा ! तेरे लिए दुनियाँ परेशान है, हैरान है, बेजान है। तू सबका सिरताज है, आफताब है, बेहिसाब है। तेरा दीदार हो जाने पर सारा आलम गफलत का ख्याले ख्वाब है। परदा फाश हो गया।
कहकहाकर बोला- अरे यार! परेशानी ही तो दुनियाँ की निशानी है और जो निशानी है वह लगबेफानी है।
बस तमाशा खतम। रहा सनम का सनम । जल गया दहरोहरम। किधर गया मक्का, किधर गया बुतखाना? खुद की नजर से देखा तो मस्तों का मयखाना।
अहा हा, वाह वाह, शिव-
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् ।
योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् ।।
अब आओ, चलो तुम्हें घुमायें। कठोपनिषद् की श्रुति कहती है-
नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ।।
(कठ. 2-6-12)
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः ।
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ।।
(कठ. 3-6-13)
क्या भाव है? नैव वाचा न मनसा-श्रुति कहती है वाणी जिसका कथन नहीं कर सकती, मन जहाँ नहीं जा सकता, दृष्टि जिसको नहीं देख सकती परन्तु अस्तीति नित्यं ब्रुवतः - है, है, है इस प्रकार रात-दिन कहता रहता है। वाणी जिसका कथन नहीं कर सकती, मन जिसका मनन नहीं कर सकता, दृष्टि जिसको नहीं देख सकती, जो इन्द्रियों का विषय नहीं है, वही कहता रहता है- है, है, है। अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते-तो फिर और कहाँ उस परमात्मा को प्राप्त करोगे? अब दृष्टि पसारकर देखो अनुभव करो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सारा चराचर कोई भी देश काल, वस्तु 'है' के बिना है? ब्रह्मादिक जिसे नहीं जान सकते। कितना ठोस भरा है, घनभूत है। ओहो! आत्म जिज्ञासुओं ! भैया ! इसको पोल न समझो, इसे पोल न मानना, इस पोल के अंदर एक ऐसी चीज है जो ठोस (घन) है, जिसमें एक पिन भी नहीं जा सकता, लबालब है, भरपूर है, कहाँ से कहाँ तक है, जो 'है' है। यही ब्रह्म सत्ता है। यही अस्तित्व है। यही नारायण सत्ता है। ओहो, कोई ऐसा काल है जो 'है' के बिना है? कोई ऐसी वस्तु है जो 'है' के बिना है। कितनी ठोस चीज है। ओहो, अब समझ लो जिस 'है' में यह है, जिस 'है' से यह है, जिस 'है' करके यह है और 'है' स्वयं ही यह है। इसी पर अनन्त विकल्पों का विकल्प है। इस सत्तापद से विकल्पों को हटा लो-बस, फिर कुछ नहीं ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सारा चराचर जिस 'अस्तित्व' पर अवलंबित है, आधारित है, जो सर्वाधार है, जो सब पर शासन करता है, जो शासकों का शासक है, जिस पर अनन्त विकल्पों का विकल्प है, वही सत्तापद है। इस पर से विकल्प हटा लो- बस, फिर कुछ नहीं। अस्तित्व मात्र ही है। जिस किसी से पूछो-कहीं पूछो- सभी यही कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के शासन में हैं, सरकार की हुकूमत है। हम सब गवर्नमेंट के नौकर हैं। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी इसी शासक के शासन में हैं। भाई! जरा हमें कोई मूर्तिवत् प्रत्यक्ष रूप से दिखाना भला कि वह शासन कौन है? जिस बंगले या कोठी में वह रहता है? जब सभी कर्मचारी हैं तो फिर गवर्नमेंट कहाँ है? सभी बताते हैं कि सरकार (शासक) बड़ी सतर्कता से सीमाओं की रक्षा कर रही है। छोटे से बड़े सभी यही बताते हैं, तो फिर हमें गवर्नमेंट का दर्शन भी करा दो। सारी दुनियाँ का शासन जो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वह कोई भी देश हो-चीन में चीनी शासन, अमेरिका में अमेरिकी शासन, पाकिस्तान में पाकिस्तानी शासन, भारत वर्ष में भारतीय शासन, सभी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चिल्लाते हैं, परन्तु गवर्नमेंट का पता ही नहीं है। ये तो सब उस शासक के कर्मचारी हैं तो शासक कहाँ है? शासक को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। यदि कहीं भी कोई पाप करेगा तो हथकड़ी पड़ जायेगी, सभी शासक से भयभीत हैं। वह शासक रूप से कहीं दिखता नहीं परन्तु शासक का डर इतना है कि नाड़ी सबकी काँप रही है। भैया ! शासक 'अस्तित्व' होता है-ठोस रग-रग में 'अस्तित्व' व्यापक है और दुनियाँ के हा एक भाग टुकड़े-टुकड़े भारत, पाकिस्तान, अमेरिका ये सभी राष्ट्र उसके हो शासन में सब काम कर रहे हैं। क्या मंत्री, क्या कमिशनर, क्या कलेक्टर, क्या चपरासी जितने भी हैं सब पर गवर्नमेंट का शासन है। सभी पर शासन कर रहा है। उसी का प्रतिपादन श्रुति कर रही है। अरे बाप रे ! उसका साम्राज्य कितना है-जो मन का विषय नहीं, मन की जहाँ गम नहीं, बुद्धि जिसको निश्चय नहीं कर सकती, दृष्टि जिसे देख नहीं सकती, परन्तु है, है रात-दिन अपने आपको कहता रहता है, तो इस अस्तित्व की 'कथं उपलभ्यते' अर्थात् और किस प्रकार प्राप्त करोगे? जबकि हर एक में जाहिर जहूर है।
नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ।।
(कठ. 3 - 6 - 12 )
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः ।
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ।।
(कठ. 3 - 6 - 13 )
बाहर भीतर लबालब परिपूर्ण है। श्रुति कहती है-उभयोः तत्वभावेन उपलब्धव्यः 'है' और 'मैं' इन दोनों को अपना आप अपना स्वरूप जानकर प्राप्त करना चाहिये। अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। 'है' 'मैं' दोनों को जो अपना स्वरूप जानता है उसके सामने तत्वभावः प्रसीदति भगवान आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। जो 'है' है 'अस्तित्व' (भगवान) वही शरीर के अंदर से अपने आपको अभिव्यक्त करता है, कहता है कि 'मैं' हूँ, 'मैं' हूँ। विद्वानों। बड़ी मजेदार चीज है-शास्त्रों के पढ़ने का यही फल है।
विद्या बिनु विवेक उपजाये। श्रमफल पढ़े किये अरु पाये ।।
अब मजा आ रहा है। अब समझ में आया भाव, इसका भाव लगा? श्रुतियों के भाव को लगा लेना कोई खालाजी का घर नहीं है। श्रुति, वेद, पुराण, गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद इन सबका भाव, बोध होने पर ही लगता है। यह बात दूसरी है कि इसके साहित्य को भले ही समझ लें, साहित्य की दृष्टि से अर्थ करके भाषण भले दे सकते हो, परन्तु भाव लगाने में तो बोधवान की ही पहुँच (गम) होती है। आजकल कॉलेजों में उपनिषत् भी पढ़ाते हैं। कई विद्वान स्वयं भी पढ़ते हैं और बड़े-बड़े आचार्य इसकी व्याख्या भी करते हैं, परन्तु भाव ग्रहण नहीं कर पाते। यदि भाव समझते हैं तो इन मंत्रों पर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? जबकि श्रुति इतनी स्पष्ट कह रही है? श्रुति क्या कह रही है। आत्मदेश का निवासी ही इसका अर्थ लगा सकता है, अन्य देश का निवासी नहीं। इसको शीघ्र समझ लेना चाहिये। अपने 'मैं' से भिन्न कुछ नहीं, यही अनन्य दृढ़ता है। अभी प्रत्यक्ष हो जाता है, अभी अनुभव होता है। हृदय में अपने आपसे भिन्न अनुभव थोड़े होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि स्वामीजी आपके समझाने से तो यही विदित होता है कि इस डंडे में भी 'मैं' हूँ। (पू. श्री स्वामी जी कहते हैं) क्या इसमें भी शक है?
एतनेहु पर करिहहिं जे संका। मोहिं ते अधिक ते जड़मति रंका ।।
'मैं' डंडे में भी हूँ। हाँ जी, हाँ है। तो फिर इसमें 'मैं' हूँ ऐसी आवाज क्यों नहीं निकलती ? बतलाते हैं? ध्यान से सुनो संसार त्रिगुणात्मक है, सत, रज और तम। तमोगुण से शरीर का निर्माण होता है, रजोगुण से इन्द्रियाँ और सतोगुण से बुद्धि। इस डंडे में तमोगुण का कार्य शरीर है-जड़ पदार्थ है, इसमें सतोगुण का अभाव है। रजोगुण नहीं इसलिए इस डंडे में इन्द्रियाँ नहीं और सतोगुण नहीं इसलिए बुद्धि नहीं है, परन्तु व्यापक तत्व चेतन इसके अंदर भी है। चेतन के दो भेद होते हैं- सामान्य चेतन और विशेष चेतन। सामान्य चेतन का प्रतीक 'है' है और विशेष चेतन का प्रतीक 'मैं' हूँ। जहाँ इस (सामान्य चेतन) को बोलने का साधन रजोगुण का कार्य इन्द्रियाँ और सतोगुण का कार्य बुद्धि मिलती है, वहीं यह अपने आपको 'मैं' इस नाम से अभिव्यक्त करता है। जहाँ पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच कोश, यह सब सामग्री एकत्र हों वहीं पर 'अस्तित्व' सामान्य चेतन परमात्मा अपने आपको विशेष रूप से 'मैं' हूँ ऐसा अभिव्यक्त करता है। इसीलिए यह चैतन्य अंदर से 'मैं' है, 'मैं' हूँ सदैव कहता रहता है। गूंगे में क्या 'मैं' नहीं हूँ? नहीं, गूंगे में भी 'मैं' हूँ, परन्तु वाणी नहीं होने से वह 'मैं' हूँ कैसे कहे? पशु, पक्षी के अंदर क्या चेतन नहीं है? क्या 'मैं' हूँ नहीं कहते? जरूर करते हैं, मगर बैखरी वाणी न होने से 'मैं' हूँ ऐसा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ठोस चीज है। इसी का नाम सेल्प रियलाइजेशन (आत्म साक्षात्कार) है। किसमें 'मैं' नहीं हूँ? किसका 'मैं' नहीं हूँ? क्या 'मैं' नहीं हूँ? सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। अब क्या कुछ बाकी है। कौन ऐसी चीज है जो मुझसे भिन्न है।
नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ।।
(कठ. 3 - 6 - 12 )
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः ।
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ।।
(कठ. 3-6-13)
आओ, दूसरी कोटि समझायें देखो इस गद्दी के पीछे पर्दा लगा है, कपड़े पर चित्र खींचा है। चित्रपट तो एक है। शीशे पर हो या पत्थर पर, कागज पर हो या कपड़े पर, चाहे दीवाल हो, इस चित्रपट पर अनेक चित्र चित्रित हैं। चित्रपट तो एक ही है, परन्तु अनेक प्रकार के चित्र इस चित्रपट पर खींचे हुए हैं, परन्तु इन अनेक चित्रों को चित्रपट से अलग नहीं कर सकते। 'अस्तित्व' आत्मा चित्रपट पर तृण से आदि ब्रह्मा पर्यन्त सारा चराचर चित्रित है। अब यह फूल है-तो 'है' हुआ चित्रपट और फूल है चित्र। इस 'है' पर हो सबका अस्तित्व है किसमें ताकत है जो 'है' को अलग करदे? शरीर है, मन है, प्राण है, इन्द्रियाँ हैं, संसार है इत्यादि विकल्प रूप सारा विश्व इस 'अस्तित्व' आत्मा चित्रपट पर ही चित्रित है। जी हाँ-
तीसरी कोटि- 'अस्तित्व' एक सम्राट सिंहासन है। जब इस सिंहासन पर 'मैं' बैठता है तो हो जाता है 'मैं' हूँ। वह और तू ये दोनों भी इस सम्राट सिंहासन पर बैठने के लिए आते हैं। वह जब इस सिंहासन के पास आता है तो वह मिटकर 'मैं' हो जाता है। तू-जब इस सिंहासन के पास आता है तो तू मिटकर 'मैं' हो जाता है। देखो-न वह रहा, न तू रहा-अरे भाई। सिंहासन पर बैठकर वह और तू अपने को 'मैं' हूँ यही कहेंगे। इसलिए वस्तुतः वह भी 'मैं' और तू भी 'मैं' हूँ। इसी का नाम गणतन्त्र है। जो जिस पोस्ट पर हो अपनी ड्यूटी करो, गणतंत्र राज्य का निवासी होकर रहना होगा। खबरदार, यह जो कुछ भी है सब गवर्नमेंट का है-जिस बंगला (कोठी, मकान) में तुम रहते हो वह तुम्हारा नहीं है, सब राष्ट्र का है, गवर्नमेंट का है। जब राष्ट्र को जरूरत पड़ेगी वह बंगला, कोठी ले ली जाएगी, किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो फिर कौन राजा, कौन महाराजा, कौन चोपदार, कौन फौजदार, सूबेदार, पोकदार सब मिट गये। एक शासन रह गया गणतंत्र। अब आ जाओ विषयपर भगवान आत्मा से किसी की भी भिन्न सत्ता नहीं है। सारे विश्व का सम्राट 'मैं' (सत्ता) इससे किसी भी चीज को अलग करो तो उसका अस्तित्व ही न रहेगा। तुम अधिक काम करते हो तो तुम्हें अधिक आमदनी होगी, परन्तु तुम्हारी या किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। 'मैं' (आत्मा) राष्ट्र में इन्द्रियाँ प्रजा हैं। मन प्रधानमंत्री है। 'मैं' आत्मा गवर्नमेंट का शासन सबके लिए है। ये आँखें देखती हैं, परन्तु यदि इनसे पूछो कि कौन है, तो आँख क्या बतायेगी? 'मैं' आँख हूँ। मैं के बिना आँख का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। यही गणतंत्र है। 'मैं' कान हूँ, मैं शरीर हूँ। बिना 'मैं' के किसी की भी सिद्धि नहीं होती। सब पर समान अधिकार है। कितना सुंदर शासन है। यह ठोस चीज है। बिना मुझ आत्मा के किसी की भी सिद्धि नहीं होती क्योंकि 'मैं' सर्वाधार हूँ, सर्व का सर्व हूँ, सर्व वस्तु करके पूर्ण हूँ, 'मैं' किसमें नहीं हूँ, 'मैं' किसका नहीं हूँ और 'मैं' क्या नहीं हूँ? लकड़ी किसमें नहीं है? चौकी में, खंभा में, तख्त में, लकड़ी किसकी नहीं है? लकड़ी सबकी है। और लकड़ी क्या नहीं है? सभी कुछ है। तो 'मैं' किसमें नहीं हूँ? किसका नहीं हूँ? क्या नहीं हूँ? कहीं भी मन का पता है? जरा मन को ढंढो न, फिर ढूँढ़ो। भैया! मन के ठेकेदार बने हो, मन की शिकायत करते हो-तो वह मन है कहाँ? जरा खोज करो-ढूँढ़ो, अरे मुबारक
हो-
है छाई दिल पे खामोशी, ये बीमारी मुबारक हो ।
ये कैसी दिल की बेहोशी, ये बीमारी मुबारक हो ।।1।।
खुशी गम बह गये दोनों, इश्क सैलाब दरिया में ।
हवायें आ रही ठंडी, ये बीमारी मुबारक हो ।।2।।
कहाँ आना, कहाँ जाना, देखना और क्या सुनना ।
सरे बाजार सन्नाटा, ये बीमारी मुबारक हो ।।3।।
ध्यान दो-जब श्री भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान मे अर्जुन को आत्म तत्व का उपदेश दिये तो दोनों तरफ असंख्य सेनायें युद्ध के लिए तत्पर खड़ी थीं, लाखों सैनिक कितना शोर हो रहा होगा, और अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठा है, भगवान एक हाथ घोड़े की पीठ पर रखे हैं, दूसरे हाथ में लगाम है और अर्जुन की तरफ मुंडी टेढ़ी करके पीछे देखते हुए उपदेश कर रहे हैं। तो फिर भगवान के गहन आत्म तत्व का उपदेश अर्जुन इतने हो हल्ला के बीच कैसे सुना? इससे जाहिर है कि हल्ला अपने देश में था, न कि भगवान देश में? यहाँ बैंड भी बजे तो बैंड की आवाज अपने देश में बजा करे। अपने देश में तो चारों तरफ सन्नाटा है। कुरुक्षेत्र का हल्ला यदि अर्जुन के देश में रहता तो इस सूक्ष्म तत्व का प्याला वह कैसे पीता? जिज्ञासुओं जिस तत्व का तुमको बोध करा रहे हैं, तो तुम्हारे आत्मदेश में सन्नाटा है, तभी उसे समझ रहे हो। हल्ला अपने देश में होता रहे। यह बालक रो रहा है तो अपने देश में रोना है आत्मदेश में? रोना देश में रोना है। तो फिर क्या रोता रहे। सरे बाजार सन्नाटा है। लहर, लहर देश में है कि जल देश में। तो लहर उठा करे। जल का क्या नुकसान है-
खुशकिस्मत से फकीरी का, खजाना मिल गया मुझको ।
जो होना है सो होने दो, ये बीमारी मुबारक हो ।।4।।
फकीरी का खजाना-क्या है? अरे भगवान की भी चाह नहीं, जिसकी ऐसी धारणा है-सचमुच में वही फकीर है। सुन लो कान खोलकर, भगवान की भी चाह जिसको न हो-वही अचाह है और यही है फकीरी का खजाना। भगवान को सब कुछ कुछ दे देने के बाद भगवान उसको क्या देता है? 'अचाह'। आत्म समर्पण कर तुमने अपने वजूद को मिटा दिया तो भगवान तुम्हें क्या देंगे? तुम्हें अकिंञ्चन बना देंगे, 'अचाह' देंगे। फिर भगवान की भी चाह नहीं रहेगी, गोविंदाय नमो नमः
दरवेशों की बातों को, समझना बूझना मुश्किल ।
कोई समझै तो क्या समझै, ये बीमारी मुबारक हो ।।5।।
दरवेश कहते हैं सिद्ध को, बोधवान को, फकीर को और दरवेश-कुत्ते को भी कहते हैं। कुत्ते में एक बड़ा गुण है-कुत्ते को प्यार करके जब बुलाते हो तो वह पूँछ हिलाकर आपके पास आ जाता है। और एक डंडा मारो तो भागता है परन्तु फिर उसे पुचकार कर बुलाओ तो वह फिर प्रेम से तुम्हारे पास आ जायेगा। दस बार मारो और दस बार बुलाओ-दस बार भागने पर भी कुत्ते के हृदय में मानापमान की लकीर नहीं पड़ती। इस तरह दरवेश (संत) का स्वभाव होता है-
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।।
जिसके हृदय में मानापमान की लकीर न पड़े वही दरवेश है। ऐसों की बातों को समझना मुश्किल है।
जहाँ में लाइलाजे मर्ज की, हिकमत न है कोई ।
मौज में चल रहे झोंके, ये बीमारी मुबारक हो ।।6।।
मुनादी मुक्त दुनियाँ में, हमेशा हो रही हरदम ।
मुबारक हो, मुबारक हो, ये बीमारी मुबारक हो ।।7।।
(मुक्तोद्गार)
------------
चतुर्थ दिवस : दूसरी बेला
दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक
श्रीकृष्ण जन्म कथा
सम्राट परीक्षित का प्रश्न श्री स्वामी शुकदेवजी के प्रति हो रहा है, राजोवाच-
कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः ।
राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् ।
यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम् ।
तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंस नः ।
अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः ।
कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात् ।।
(श्रीमद्भा. 10/1/1-3)
सोम सूर्ययोः उभयवंश्यानां राज्ञां परमाद्भुतम् चरित एवं वंश के विस्तारः भविता कथितः। सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों वंश के राजाओं के सुंदर अद्भुत चरित्र और वंश विस्तार श्रीमद् भागवत के नवम् स्कन्ध तक आप सुना चुके हैं। धर्मशीलस्य यदोः धर्मशील धर्मनैष्ठिक महाराजा यदु के वंश में भूतभावन भगवान विश्वात्मा अवतार लेकर जो भी चरित्र किए हैं वह कृपा करके कहिये-
निवृत्ततवर्षैरुपगीयमानाद् भवौषधाच्छ्रोत्रमनोऽभिरामात् ।
क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् ।।
(4 - 1 - 10)
उत्तमश्लोकगुणानुवादात, कृष्णचरितात अस्मिन् संसारे इतिभावः कः पुमान विरज्येत, को अर्थः कोऽिप न विरक्तं कुर्यात उत्तम श्लोक जो भगवान कृष्ण हैं का जो चरित्र है गुणानुवाद उससे संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे वैराग्य हो, प्रायः सभी श्रवण करते हैं, क्योंकि 'संसारे त्रयः श्रोतारः संन्ति'- संसार में तीन प्रकार के श्रोता होते हैं-' भक्ताः मुमुक्षवः एवं विषयेनः'-' भक्त मुमुक्षु एवं विषयी' जे भक्ताः तेषां कथं कृष्ण चरित? उपगीयमानं। जे मुमुक्षवः तेषा कथं? भवौषधं और जे विषयेनं तेषा कथं? मनोभिराम। जो भक्तगण हैं उनके लिए भगवान का चरित्र कैसा है?' श्रृण्वन्ति गायन्ति साधवः' प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं? और भक्तजनों के बीच बैठकर इसका उपगायन करते हैं और जो मुमुक्षु है, मुमुक्षुओं के लिए कैसा है कि भव औषध है। 'भवन्ति जनः अस्मिन संसारः तस्य औषधाम भवऔषधम।' संसार जो आवागमन का रोग है उसके नाश के लिए यह भवऔषध है, दवा है। और जो श्रृंगारी है........ उनके लिए मनोभिराम है, मनोरंजन है, परंतु ऐसे भी जिनको भगवान का चरित्र अच्छा नहीं लगता है, वो कैसे है? अपशुध्नात बिना अपगतः शुकः शोको जस्मात् स आत्मा तं हन्ति इति पशुध्नात विनः। शास्त्र में भगवान आत्मा का विश्लेषण अपशुक दिया है, अपशुक का मतलब ये होता है 'तरति शोक आत्मवित' विद्वान शोक मोहौ जहाति। जो आत्मा को जानता है, अपने स्वरूप जो चराचर का अस्तित्व है-उसे जो जान लेता है, अनुभव कर लेता है वो शोक मोह से तर जाता है। तो जिसको जान करके शोक मोह नष्ट हो जाय इसलिए भगवान आत्मा को अपशुक कहा है। जो अपशुघ्नि है, आत्मध्नि है, आत्म वंचित है उन्हीं को भले ही भगवान का गुणानुवाद प्रिय न लगे और बाकी तो सभी श्रवण करते हैं। अब प्रश्न होता है कि आत्मा तो अजर-अमर, अविनाशी है तो आत्मा का हनन तो कोई कर नहीं सकता तो व्यक्ति का नाम आत्मघ्नि कैसे हुआ? इस पर कहते हैं।
नृदेह माद्यं सुलभं, सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम ।
मयानुकूलेन नभस्वतेरित पुमान् भवाब्धिम् न तरेत्स आत्महा ।।
जिस प्रकार नदी पार करने के लिए इतनी सामग्री की जरूरत पड़ती है- नाव, पतवार, केंवट और अनुकूल वायु। इसी तरह संसार रूपी नदी पार करने के लिए ये शरीर है, यही नाव है और श्रद्धा ये पतवार है। गुरु जो है, कर्णधार केंवट है और भगवान की जो कृपा है यही अनुकूल वायु है। ऐसा सुंदर सुलभ साज पाकर जो न तरा स आत्मघ्न वही आत्मघाती है।
नर तन भव बारिध कहँ बेरो ।
सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो ।
करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा ।
दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ।
जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाय ।
सो कृत निदंक मंदगति आत्महन गति जाय ।।
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्वतया ।
देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं बिना ।
(10.1.8)
कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाद व्रजं गतः ।
क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतांपतिः ।।
(10.1.9)
भगवान जिस दिन अवतार लिये हैं उसी दिन गोकुल को चले गये अथवा कुछ दिन रहकर के गये हैं और वहाँ कितने दिन रहे और वहाँ क्या-क्या चरित्र किये, वहाँ से मथुरा कब आये, मथुरा से द्वारिकापुरी कब गये इत्यादि ।
एतदन्यश्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितम ।
वक्तुमर्हसि सर्वज्ञश्रद्दधानाय विस्तृतम् ।।
जो कुछ पता था सो तो मैंने पूछा बाकी भगवान तुम तो सर्वज्ञ हो। शुकदेव स्वामी ने कहा तुम ये तो बताओ भगवान के और बहुत से अवतार हुए हैं और अवतारों के संबंध में तुम्हारा प्रश्न नहीं होता, चरित्र सुनने की इच्छा तुम्हें नहीं होती, भगवान श्रीकृष्ण के ही चरित्र सुनने की इच्छा क्यों करते हो? क्या बात है? परीक्षित कहते हैं- भगवन् ! बात ये है कि भगवान कृष्ण हमारे परम पूज्य हैं, हमेशा से हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। (शुकदेव जी पूछते हैं कि) कब और कैसे रक्षा किये? तो कहते हैं-
पितामहा मे समरेऽमरञ्जयै देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः ।
दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं, कृत्वातरन् वत्सण्दं स्म यत्प्लवाः ।
दौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम् ।
जुगोप कुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः ।।
(10-1-5)
परीक्षित कहता है 'मे पितामह पाण्डवाः समरे संग्रामे अमरञ्जयैः' परंतु 'कौरव सैन्य सागर दुरत्ययः ।'
महाभारत में मेरे पितामह जो थे पाण्डव वो देवताओं को भी जीतने वाले थे-'अमरजैः' थे परन्तु कौरवों की जो सेना थी वो सागर रूप थी। वो कहते हैं कि समुद्र में तो बड़े-बड़े मत्स्य होते हैं।
तिमिर नाम शत जोजन विस्तरः तिमिगिलोसति... ।।
समुद्र में एक तिमिर नाम का मत्स्य होता है जो सौ योजन वाले मत्स्य को निगल जाता है। जब कौरवों की सेना समुद्र के समान थी तो बड़े-बड़े मत्स्य कौन थे? देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः ।
देवव्रत माने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब मत्स्य के समान थे।
यद्यपि मे पितामयः अमरंजै परंतु कौरव सागरं न पार कर्तुं समर्थः ।।
यद्यपि हमारे पितामह 'अमरजैः' थे परंतु कौरव सैन्य सागर को पार करने में यानि जीतने में समर्थ नहीं थे। भगवान् श्रीकृष्ण के असीम कृपा से गोवत्स पद के समान अट्ठारह दिन में ही पार कर गये अर्थात् विजय प्राप्त किये। भगवान ने तुम्हारी रक्षा कब की तो कहता है-
द्रौणयस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम् ।
जुगोप कुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः ।।
(6 - 1 - 10)
द्रोणस्योत्पतिं द्रोणी अश्वथामा ते ब्रह्मास्त्रेण गर्भाशये संतानबीजं
कुरुपाण्डकांनाम । विप्लुष्टं तं काले शरणं गतायाः उत्तरा कुमारयाः ।।
आत्तचक्रः को अर्थ गृहीता चक्रेण योनः श्रीकृष्णः भगवतः
कुक्षेण गतः मां परीक्षितं जुगोप कुक्षिं को अर्थ रक्ष ।।
द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी अश्वथामा जो था कौरवों का पक्षपाती और दुर्योधन का घनिष्ट मित्र था। महाभारत समाप्त हो जाने पर कौरव-पाण्डव दोनों का संतान बीज मैं परीक्षित उत्तरा के गर्भ में अवशेष रह गया था। मेरे पिता अभिमन्यु भी चक्रव्यूह भेदन में मारे गये थे। उस समय उसने (अश्वत्थामा) सोचा कि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूँ और गर्भ में स्थित जो गर्भस्थ बालक है ये भी नष्ट हो जाये। उस समय उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मेरा शरीर गर्भाशय में जलने लगा। मेरी माँ उत्तरा भगवान के शरण में गई। उस समय भगवान श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्रधारी माता के गर्भ में जाकर के सुदर्शन चक्र से भगवान ने ब्रह्मास्त्र का नाश किया और जब तक मैं पैदा नहीं हुआ तब तक निरंतर मेरी रक्षा के निमित्त भगवान को भी उतने दिन गर्भ में रहना पड़ा। इसलिए भगवन् ! भगवान श्रीकृष्ण का चरित्र हमें बड़ा ही प्रिय है। आप सुनाइये कृपा करके। जब सब प्रश्न परीक्षित के हो गये-
एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं, वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम् ।
प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलि कल्मषघ्नं, व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः ।।
(10 - 1 - 14)
वैयासकी: भगवान शुकदेवः एवं निशम्य को अर्थ श्रुत्वा साधुवाद प्रकृन, प्रत्यर्च्य को अर्थः प्रसंस्य कले: कलसंतापं हन्ति इति कलिकल्मशघनं कृष्णण चरित व्याहुर्त कथितं भागवत प्रधानं भगवानः शुकदेवः आरभत ।।
राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर स्वामी शुकदेव बड़े प्रसन्न हो गये और भगवान कृष्ण के जो चरित्र हैं, कलिमघ्न कलि के पापों का नाशक कहने के लिए आरंभ कर दिये। धन्य हो परीक्षित ! भगवान वासुदेव की कथा में तुम्हारी ऐसी अनन्य प्रीति क्या कहना।
वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषांस्त्रीन् पुनाति हि ।
वक्तारं पृच्छकं श्रोतृस्तत्पादसलिलं यथा ।।
(10 - 1 - 16)
अच्छा तो फिर अब सुनो भगवान का चरित्र हम सुनाते हैं।
भूमिर्दृप्त नृपव्याजदैत्यानीक शतायुतैः,
आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ।
गौर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विभोः,
उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत ।।
(17-1-10)
जब अत्याचारी राजाओं के अत्याचार से पृथ्वी भारायमान हो गई-न सह सकी, उस समय गौ का रूप धारण कर बिलखती हुई ब्रह्मा के शरण में गई। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने पूछा बंसुन्धरे । कैसे आई तू? तो पृथ्वी कहती है- गिरी सरि सिंधु भार नहीं मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ।।
महाराज मुझ पृथ्वी पर अनेक सागर, अनेक पर्वत, अनेक नदियाँ हैं। इनसे मुझे कोई भार नहीं, परंतु यदि कोई व्यक्ति परद्रोही है, ईर्ष्यालु, परनिंदक है तो एक ही व्यक्ति का भार सहन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ।
ब्रह्माजी ने निर्णय किया कि अब देवताओं को बुलाना चाहिए, तो भगवान ब्रह्मा सब देवताओं को इकट्ठा किये। सभा लगी उस सभा के सभापति भगवान ब्रह्मा हुए। विषय रखा गया सभा में कि भाई जितने भी देवता हों अपनी-अपनी राय दो, हमको, भगवान की स्तुति करने के लिए कहाँ चले। इस कथानक की भगवान शंकर माता पार्वती से कैलास में कह रहे हैं-
बैठे सुर सब करही विचारा कहँ पाइअ प्रभु करहि पुकारा ।
पुर बैकुंठ जान कह कोई काऊ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ।।
किसी देवता ने ब्रह्माजी को राय दिया कि बैकुंठ चले। वहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, किसी देवता ने कहा क्षीर सागर चलना चाहिए वहाँ भगवान शेषनारायण रहते हैं। माता जी सुन रही थीं। माताजी ने पूछा भगवन ये तो बताओ क्या उस जमाने में भी इलेक्शन की बीमारी थी? कोई बैकुंठ की पेटी में वोट डाल रहा, कोई क्षीर सागर की पेटी में वोट डाल रहा है। बात क्या है? क्या उस जमाने में भी मतभेद था? भगवान शंकर ने कहा- नहीं मतभेद का तो कोई काम नहीं। फिर-
जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहं प्रगट सदा यह नीति ।।
माताजी ने कहा- महाराज आप भी तो थे न उस सभा में तो आपने फिर अपनी राय क्या दिया। भगवान कहते हैं, सुनो-
तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ, अवसर पाई वचन एक कहेऊँ ।
मुझे भी मौका मिला बोलने का। सभापति ब्रह्मा का दृष्टिपात एकाएक मुझ शंकर पर हुआ। तब उन्होंने कहा- देवताओं, सबने तो अपनी-अपनी राय दी परंतु भगवान शंकर भी तो यहाँ बैठे हैं, उनकी भी तो राय ले लेनी चाहिए, वो कहाँ जाने को कहते हैं? शंकर जी कहते हैं- मुझे मौका मिला बोलने का तब मैंने क्या कहा-
सभी उपस्थित सभा सदस्यगण देववृन्द एवं सभापति महोदय भगवान ब्रह्मा! यदि मुझ शंकर की राय ली जाती है तो मैं यही कहूँगा कि क्षीरसागर और बैकुंठ जाने की कोई आश्यकता नहीं। क्योंकि -
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि हम जाना ।।
कहीं जाने की जरूरत नहीं परमात्मा भरपूर है। सर्व देश करके पूर्ण, सर्व काल करके पूर्ण, सर्व वस्तु करके पूर्ण तिलभर जगह जिससे खाली नहीं है और फिर 'समाना' ऐसी बात तो है नहीं कि भगवान यहाँ पर एक किलो हों और वहाँ पर एक छटाक समान यानि बराबर एक-सा, जी हाँ! अरे भाई। भगवान पर बैठे हो, बैठकर कथा सुन रहे हो। अरे कहो जमीन में बैठे हो। जहाँ जमीन में बैठे हो, भगवान नहीं है क्या? कह दो किसी के हृदय में साहस हो तो जहाँ हम बैठे हैं, भगवान नहीं है। ऐसे में तो भगवान का व्यापकपना असिद्ध हो जायेगा। वो जगह भगवान से खाली हो जायेगी। भगवान पर ही बैठे हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो सब भगवान। सर्वत्र भगवान सब कुछ भगवान-
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई हम जाना ।
देश काल दिशि विदिशहू मांही कहहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ।
अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी ।।
सर्व देश करके पूर्ण, सर्व वस्तु करके पूर्ण, मगर कालान्तर में, देश काल वस्तु का नाश हो जाता है। देश, काल, वस्तु में व्यापक परमात्मा का देश काल वस्तु के नाश होने में यानि जिसमें परमात्मा व्यापक है, उस व्यापक के नाश होने में क्या परमात्मा का भी नाश हो जाता है? तो भगवान शंकर कहते हैं, नहीं 'विरागी।'' अग, जगमय सब रहित विरागी', विरागी माने असंग सब में रहते हुए भी 'निर्लेप' हैं।
माताजी ने पूछा- जब आपने ऐसा कहा तो आपके कथन का किसी ने विरोध किया? भगवान शंकर कहते हैं-नहीं, विरोध कौन करेगा? किसकी ताकत है, विरोध करने की। तो फिर क्या हुआ? अरे हुआ क्या-
मोर वचन सबके मन माना, साधु-साधु कहि ब्रह्म बरवाना ।।
सर्व सम्मत से प्रस्ताव पास हो गया। भगवान शंकर ने जो कुछ कहा है, सब ठीक है, कहीं चलने की जरूरत नहीं। चारों तरफ से धन्यवाद, धन्यवाद की आवाज, थैंक्यू-थैंक्यू, चारों तरफ से जिधर देखो-उधर पास हो गया प्रस्ताव ।
हाँ, पुराणों में, रामायण में, जहाँ कहीं भी ज्ञान का प्रसंग आता है, वहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती जी के संवाद में आता है। भगवान शिव जो हैं कल्याण स्वरूप कहे जाते हैं, साक्षात् आत्मा हैं। शिव माने साक्षात् आत्मा के कल्याणे धातु से 'शिव' शब्द बनता है। है जिसे सभी मानस प्रेमी पढ़ते हैं-
औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि ।
संकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरि ।।
(रा.उ.कां. 451)
भगवान राम कहते हैं क्या गुप्त मत है, प्रगट मत नहीं-
औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि ।
शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरि ।।
'शं कल्याणं करोति इति शंकरः', 'शं' माने कल्याण और 'कर' माने करने वाला तो बिना अपने स्वरूप भगवान आत्मा को जाने कल्याण तो होता ही नहीं। तो शंकर नाम आत्मा का है। बिना अपने स्वरूप को जाने, भगवान राम कहते हैं, मेरी भक्ति नहीं पा सकता। यही गुप्त मत है और एक गुप्त- सबहिं कहउँ कर जोरि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरि ।।
हाँ जी, तो सभी देवता मिल करके 'पुरुषसूक्त' मंत्र से भगवान की स्तुति किए, उस समय आकाशवाणी हुई-
गिरं समाधौ गगने समीरितां, निशम्य वेधास्त्रि दशानुवाच ह ।
गां पौरुषीं मे श्रृणुतामराः पुनर्विधीयतामाशु तथैव मा चिरम् ।।
(10.1 21)
पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो, भवद्भिरंशैर्यदुषूपजन्यताम् ।
स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद् भुवि ।।
(10.1.22)
पौरुषी वाणी हो रही है। ब्रह्माजी ने किस समय सुना? समाधि काल में-
गिरं समाधौ गगने समीरितां, निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच ह ।।
भगवान ब्रह्मा पौरुषी वाणी सुनकर, देवान प्रति उवाच- देखो भाई, आकाशवाणी हो रही है, इसको मैं समझेंगा और जो तुम लोगों से कहूँगा उसे भूलना नहीं-
पुरैव पुंसावधृतो धरा ज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुपूप जन्यताम् ।
स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपर्यश्चरेद् भुवि ।।
'धरा' जो पृथ्वी है उसको जो कष्ट है, उसके निवारण के लिए अवतार अवश्यमेव होगा।
वसुदेव गृहे साक्षाद् भगवान् पुरुषः परः ।
जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुर स्त्रियः ।।
(10.1.23)
वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार अवश्यमेव होगा। योगमाया के द्वारा संसार को निश्चय होगा कि कहीं न कहीं अवतार अवश्य हो गया। आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा आश्वासन मिला। देवता अपने-अपने स्थान पर आ गये। कालान्तर में उग्रसेनी कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव से किया और बहुत कुछ दहेज देकर विदा करने जा रहा था। उस समय अब कंस के लिए आकाशवाणी होती है। कंस !
अस्यास्त्वामष्टमो गर्भा हन्तायां वहसेऽबुध ।
(10.1.34)
अरे अबोध मूर्ख कंस !
'अस्याः देवक्याः अष्टमो गर्भाः त्वां हन्ताः' जिस प्रसन्नता के साथ तू आज अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा है, अरे! इसी का जो आठवाँ गर्भ होगा वो तेरा काल होगा, उसी के हाथ तेरी मृत्यु निश्चित है। कंस सुना और सुन करके रथ से उतर पड़ा और देवकी का केश पकड़कर पटक दिया पृथ्वी पर और निकाला खड्ग और इस दुष्टा को मार डालूंगा कहा। उस समय महात्मा वसुदेवजी विचार करने लगे, अभी तो ये मूर्ख बड़ा प्रसन्न था, अब क्या हो गया इसको? तो वसुदेव जी कहते हैं-
श्लाघनीयगुणः शुरैर्भवान् भोजयशस्करः,
स कथं भगिनी हन्यात् स्त्रियमुद्वाहपर्वणि ।।
(10.1.37)
भोजराज ! अभी तो तुम बड़े प्रसन्न थे, ऐसे विवाह के मंगलमय पर्व पर अपनी बहन देवकी को भैया क्यों मारते हो? क्या बात है? कंस ने कहा-चुप रहो ! अभी आकाशवाणी हुई है देवकी का आठवाँ गर्भ मेरा काल होगा इसलिए दुष्टा को नहीं छोडूंगा मार डालूंगा पापिनी को। वसुदेवजी ने कहा ठीक है, परंतु सोचो तो सही -
मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते,
अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः ।।
(10-1-38)
हे वीर ! 'जन्मतां देहेन सह जायते मृत्यु।' जन्म लेने वालों के साथ में अर्थात् देह में मृत्यु भी पैदा होती है। ये न समझना चाहिए कि मरने के समय मृत्यु कहीं बाहर से आती है। गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यन्त चौबीस घंटा देह और मृत्यु का वियोग कभी होता ही नहीं।
अरे! जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसकी आयु घटने लगती है। अज्ञानता के कारण माता-पिता प्रसन्न होते हैं कि अब मेरा बच्चा घुटने के बल चलने लगा, बड़ा हो गया। अब दौड़ने लगा, अब बोलने लगा, अब ये विचार करो कितने दिन की उमर घट गई उसकी। अरे भाई। जिस दिन से बच्चा बाहर आता है उसी दिन से तो उसके आयु का हिसाब होगा न? अरे उसी दिन से हिसाब लगेगा भाई। पाँच सालका बालक हो गया तो पाँच साल की उसकी उमर घट गई। दस साल का हुआ तो दस साल की उमर घट गई। उमर तो उसकी घट रही है न। तो अफसोस के बदले दुनियाँ हँसती है। कैसी उल्टी खोपड़ी है। अरे उसी दिन से रोना शुरु करे। मगर ये बात कोई फक्कड़ ही कहेगा। हाँ! और सबकी हिम्मत नहीं कहने की। जिस दिन पैदा हुआ, उस दिन से रोना शुरू कर दे। रोना तो एक दिन है ही, मरने के बाद, उसी दिन से शुरू कर दे रोना, क्योंकि उमर घट रही है धीरे-धीरे। अरे मृत्यु साथ में नहीं है तो जैसे बालक पैदा होता है वैसे ही रहना चाहिए। मृत्यु जो है जैसे दीमक कौड़ा लकड़ी को खाता है वैसे ही चुन रही है।
मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सह जायते ।।
अच्छा! और जो कोई पैदा होता है न वो जीने के लिये पैदा नहीं होता मरने के लिए पैदा होता है। जो जन्म लेता है वो मरने के लिए। जी हाँ! अरे जब मरने के लिए ही पैदा होना है तो वो आज मरे या शतान्ते सौ बरस बाद माना तो है ही, तो अफसोस करने की क्या जरूरत है।
मृत्युजन्मतां वीर देहेन सह जायते ।।
देखो न ! जब छोटे-छोटे बच्चे जब बड़ों को प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं तो बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं-जीते रहो बेटा! अगर मरने की शंका नहीं तो आशीर्वाद की क्या जरूरत। जीते रहो बेटा। या अरे यार व्यवहारिक शब्दों में ये रहस्य भरा हुआ है। कोई समझे तो समझे। जीते रहो बेटा ! तुम्हारे आशीर्वाद से जीता रहेगा? उसे तो मरना ही है एक दिन। कोई भी आशीर्वाद दो मरना ही है, पैदा जो हुआ है। इन बातों को अगर समझ लिया जाय, अच्छी तरह से ये बातें दिमाग में बैठ जाये तो दुनियाँ मर जाये कभी आंसू न बहे। दुनियाँ पागल हो जाती है।
मृत्युर्जन्मतां वीर देहेन सह जायते ।
अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः ।।
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः ।
दहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ।।
(38.1.10)
वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को कि 'देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कमिनुगोऽवशः' - देही जीव-देही जो जीव है, जो देह धारण करे उसका नाम देही। देही जो जीव है अरे कर्मानुगुः इसका नाम है कर्मानुग। जीव को कहते हैं कर्मानुगु। 'कर्माणाम अनुपश्चात् गच्छिति इति कर्मानुगः' - कर्मों के जो पीछे-पीछे चले घसीटता फिरे, घसीटा जाय, इसीलिए इसका नाम कर्मानुग। देखो कर्तापने, भोक्तापने के अंहकार को लेकर जो भी कर्म किया जाता है वह सभी कर्म जीव के ही किये हुए, जीव को अनेक योनियों में घसीटकर ले जाता है। हालांकि जीव जाने की इच्छा नहीं करता मगर करे क्या? 'अवशः' विवश होकर के मजबूरी से जाना ही पड़ता है, रोकर जाये या हँसकर। कमाई जो किया है, भोगेगा कौन? जी हाँ ! बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में परतंत्र है। स्वतंत्र नहीं है।
कोई भी व्यक्ति चोरी करता है। चोरी करने में तो स्वतंत्र है। एक पैसा चोराये या लाख रुपया स्वतंत्र है वो पर कोई चाहता है हमें सजा मिले हमारे हाथ-पैर में हथकड़ी बेड़ी पड़े? कोई नहीं चाहता पर फल भोगने में, सजा भोगने में परतंत्र है। चाहे रोकर सजा भोगे या हँसकर। इसी तरह से जीव के ही किये हुए अहंकारवश, जो कर्म है वे कर्म जीव को घसीटकर ले जाते हैं। और इसको भोगना पड़ता है और जो अपने आपको जानता है कि मैं चराचर का अस्तित्व हूँ, व्यापक तत्व 'मैं' आत्मा हूँ। इस समझ में इस ज्ञान में, इस अनुभूति में जो कर्म करता है वो कर्म को घसीटकर, समेट कर ले जाता है। अब जो तुम्हें पसंद हो चुन लो भैया।
अगर घसीटू बनना है तो अपने आप को जीव मानो, जीव मानकर कर्म करो और कर्म को घसीटना है तो फिर अपने आप को भगवान आत्मा जानो, उसमें कहना ही क्या है। बिल्कुल। आत्मवेत्ता पुरुष भी कर्म करता है, जो अपने आपको आत्मा जानता है। वह भी कर्म करता है और जो अपने आपको जीव मानता है अरे ! जो अपने आप 'मैं' को आत्मा जानता है वह भी कर्म करता है और अपने 'मैं' को जो जीव मानता है वह भी कर्म करता है। मगर मानने में घसीटू है, जो अपने आप को 'मैं' को व्यापक तत्व आत्मा जनता है वह कर्म वो भी करता है मगर कर्मों में ताकत नहीं कि उसे घसीट सके, क्योंकि उसके किये हुए कर्म भुने हुये चने के समान हैं। जी हाँ! फुटाने हैं! जली हुई रस्सी के समान हैं। रस्सी जब जल जाती है वो राख भी टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देती है, मगर वो बंधन का कारण नहीं होती। इसी तरह से आत्मवेत्ता पुरुष के जो कर्म होते हैं, आत्मनैष्ठिक के जो कर्म होते हैं, बोधवान के जो कर्म होते हैं, वो जली हुई रस्सी के समान होते हैं, वो कर्म उसे बंधन में नहीं डालते। जीव के कर्म कच्चे दाने हैं और आत्मनैष्ठिक के कर्म भुने हुए दाने हैं। फुटाने हैं!
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः ।
दहोन्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ।।
(10-1-39)
व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति,
यथा तृणजलूकैवं देही कर्मगतिं गतः ।।
(10 - 1 - 40)
एक देह से दूसरे देह में जाना ! परंतु किस तरह से? 'प्राप्तनं वयुः त्यजते ।' पहले इसका संकल्प पहुँच जाता है, जहाँ जाना होता है, जीव को। तब 'प्राक्त' याने पूर्व का जो शरीर है, जिसमें है, उसको त्याग करके जाता है। 'देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः' 'देहान्तर मनु प्राक्तनं त्यजते वपुः। व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवेकेन गच्छति ।'
जिस तरीके से एक तिलजऊ का होता है। कीड़ा घास के ऊपर का ऐसा (स्वामी जी ऊंगली दिखाकर बता रहे हैं) चलता है वो आगे का सहारा जब उसको मिल जाता है, तब पिछड़ा धड़ उठाता है। इसी तरह से जीव को कर्मानुसार जहाँ भी जाना है। देखो ये जो बताई जा रही है कर्म फिलॉसफी है, यहाँ विचार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। विचार करोगे तो सारी पोल खुल जायेगी। शास्त्र जैसा बताते हैं उसी के अनुसार आँख मूंदकर चलना है।
क्योंकि, अनुभव करने पर, विचार करने पर सिवाय स्वस्वरूप भगवान आत्मा के कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो जैसा सुना जाय वैसा ही देखा जाये। जी हाँ! ये जो स्वस्वरूप है इसे जैसा सुनो, वैसा देखो। जब चाहो तब देखो, जहाँ चाहो वहाँ देखो, जैसा चाहो वैसा देखो। जब चाहो तब देखो-एक ! सबके भाव अलग-अलग हैं। जहाँ चाहो, वहाँ देखो और जैसा चाहो वैसा देखो। देह देखो ! जीव देखो! है देखो! नहीं देखो ! ये तुम्हारी मर्जी है। जब चाहो, तब देखो। हाँ! भगवान नगद धर्म है, उधार धर्म थोड़े ही है। जब चाहो तब देखो और जहाँ चाहो वहाँ देखो। घर में देखो, वन में देखो। जब चाहो, तब देखो। सुबह देखो, शाम को, आधी रात को। तो जब चाहो, तब देखो और जहाँ चाहो वहाँ देखो। वन में देखो, पहाड़ में देखो, जंगल में देखो। घर में देखो, पंडाल में देखो, सड़क में देखो। अरे, मैं कहाँ नहीं हूँ और जैसे चाहो वैसे देखो। चाहे साढ़े तीन हाथ का देखो, चाहे जीव रूप में देखो। चाहे है देखो, चाहे नहीं देखो। जैसे चाहो वैसे देखो।
भैया ! ऐसा पदार्थ सिवाय भगवान आत्मा के दूसरा है ही नहीं। हाँ ये बात है। परन्तु, बाकी तो सब तथ्यहीन है। हाँ, आस्तिक देश में, आस्तिक परिवार में और आस्तिक समाज में पैदा होने के नाते वेद, शास्त्र जैसा बताते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। (धीरे से) इस टोन में कहो ललकार के न कहो। अब भाव प्रदर्शित हो गया। हाँ, विश्वास करते हैं। परन्तु, अगर इसके अंदर घुसो तो सब पोलमपोल है। कहना ही कहना है। अंदर घुसोगे तो सब कहानी है। कुछ न मिलेगा तुम्हें। सब कहानी है, शंख ढपोरी है। सुनावें का? हाँ, एक दृष्टांत है, शंख ढपोरी का, एक कोई गरीब ब्राह्मण था। क्योंकि बेचारा दरिद्र था, उसने गंगा मैया की तपस्या की। गंगाजी प्रसन्न हुई तो छोटा-सा एक शंख दिया और गंगा जी से ये वाणी सुनाई पड़ी। अरे, ब्राह्मण ये शंख तुझे मैं वरदान के रूप में दे रही हूँ। इसे ले जा और संध्या वंदन के समय जब इसकी पूजा करेगा। इससे पाँच रुपया निकलेगा, चांदी का सिक्का। इससे तेरा निर्वाह हो जायेगा, जा मैं प्रसन्न हूँ। अब ब्राह्मण समझ गया डेढ़ सौ रुपये तो लग ही गया। उस वक्त इतनी महंगाई थी नहीं। अब ब्राह्मण शंख लेकर पैदल चला अपने घर को। पहली मंजिल आई तो एक सेठ की दुकान थी वहाँ पर उतरा सामने मंदिर था, बाग-बगीचा बड़ा सुंदर स्थान था। ब्राह्मण सोचा अभी तक नहाये-धोये नहीं हैं। चलो, यहीं पर स्नान पूजा करके चले जायेंगे। जब ब्राह्मण अपना थैला उतारने लगा, सेठ गद्दी पर बैठे देख रहा है, मुटुर-मुटुर। ये महाराज, क्या है भाई! यहाँ जगह नहीं हे, चलो गाँव के बाहर बगीचा है वहाँ ठहरो, चलो आगे। ब्राह्मण ने कहा कि सेठ जी हम तुमसे खाने-पीने की थोड़ी मांगेगे, टाइम हो गया है, स्नान का। स्नान, संध्या पूजन करके चले जायेंगे। चलो यहाँ जगह नहीं, सेठ ने कहा। बहुत कुछ प्रार्थना किया ब्राह्मण ने, बेचारा भूखा-प्यासा था, कुछ खाया-पिया नहीं था। अच्छा, देखो जल्दी पूजा-पाठ करके चले जाना यहाँ से रहना नहीं। ब्राह्मण-पूजा पाठ किया और वो प्रार्थना किया। जय हो महाराज! कृपा करो। पाँच रुपया खन्न से निकला। जब पाँच रुपया खड़का निकला तो देख लिया बनिया दूर से- 'ये चीज है मारने लायक।' अब ब्राह्मण तो प्रसन्न हो गया कि गंगा जी का वरदान तो सत्य है। चलो पाँच रुपया तो हमें रोज मिला करेगा। अब पाँच रुपया तो रखा अंटी में और जल्दी झोला तैयार करके चलने लगा, तब बनिया दौड़कर दण्डवत् प्रणाम किया। जय हो महाराज ! ऐसे बिना खाये-पीये चले जाओगे तो हमारा नाश हो जायेगा। क्षमा करना हमें क्या पता था आप ऐसे सिद्ध पुरुष हैं। ठहरिये, बिना भोजन कराये नहीं जाने देंगे, आपको और आज ठहरिये यहाँ। ब्राह्मण सीधा-सादा तो था ही, बेचारा ठहर गया। अच्छा, महाराज क्या बनाओगे? पूड़ी-साग, कि खीर, कि दाल-भात, रोटी-सब्जी जो मर्जी आये आपकी कृपा से सब कुछ है। अरे पुसौवा, ला रे महाराज के लिए पूड़ी-सब्जी का इंतजाम कर जल्दी। अब महाराज, पूड़ी-सब्जी वगैरह सब खूब घोटे। ईमानदारी छोड़कर खूब खाये और खाकर आसन बिछाकर सो गये। बनिया देखता रहा पाँच रुपया देने वाला शंख इसी झोले में है। सो गया महाराज ! तब रात बारह- एक बजे सेठ उठा, उसके यहाँ ठाकुर द्वार था। ठाकुर द्वार में शंख था, बिल्कुल वैसे नमूने का, अपने घर वाला शंख तो रख दिया। ब्राह्मण के झोले में और पाँच रुपया देने वाला शंख था उसे उठा ले गया। ब्राह्मण बेचारे को क्या पता खूब खाया और सोया। जब चार बजा ब्राह्मण झोला रखा और अपने घर का रास्ता पकड़ा।
जब घर पहुँचा फिर दूसरे दिन माने वही जैसे पूजा करके शंख से मांगा था। जय हो महाराज ! जय हो देवता! देव महाराज ! कृपा करो। वो तो देने वाला शंख तो था नहीं, नकली शंख था। अब घंटों विनती करता रहा। रोता रहा, कौन दे। ब्राह्मण तो अधमरा सांप हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्या हो गया। एक ही दिन पाँच रुपया दिया, अब देता ही नहीं। तो फिर बेचारा गया गंगाजी के पास। रोया महारानी गंगा माता एक ही दिन दिया पाँच रुपया, तुम्हारा शंख अब देता ही नहीं। तब गंगा जी से आकाशवाणी हुई। ऐ ब्राह्मण तू ठगा गया है रे ! वो शंख अब तुम्हारे पास नहीं रहा उसे किसी ने ले लिया। वो नकली शंख है, ये थोड़े ही देगा पाँच रुपया। गंगाजी ने कहा देख ये मैं दे रही हूँ, एक दूसरा बड़ा शंख, इसका नाम है ढपोरशंख। इसे ले जा और जहाँ पर पहले ठहरा था रात वहीं ठहरना। ये जितना मांगेगा उसका दस गुना देने को कहेगा, मगर देगा एक पैसा नहीं। लेके चला ब्राह्मण शंख इतना भारी था कि उसे लेकर चलते-चलते ब्राह्मण हाँफ गया, जी। अब ब्राह्मण उसी मुकाम पर जा ठहरा। सेठ फिर दण्डवत् प्रणाम किया। जय हो महाराज ! बड़ी जल्दी कृपा किये देवता। ब्राह्मण अपना नहाया धोया। नहा धोकर फिर शंखढपोर की पूजा करके फिर मांगा शंखठपोर से। जय हो महाराज ! दे एक हजार रुपया। क्योंकि, गरीब बेचारा ब्राह्मण कितना मांगे। एक हजार ही काफी है। तो शंख ढपोर जोर से आवाज देकर कहता है-ले रे ब्राह्मण दस हजार। अब तो बनिया सोचा। ये है काम की चीज।
उसने क्या किया ले महाराज देवता आज क्या बनाओगे? ब्राह्मण बेचारा क्या करें, जब तक काम न हो जाये ठहना ही है, उसको। फिर माल घोटा। अब सोकर के शंख ढपोर को अपने सिराहने किनारे में रख दिया। और रात भर नींद न आयी ब्राह्मण को ऐसे टटोलता है कि माने वो शंख हमारा आया कि नहीं नींद न आयी बेचारे को। रात बारह-एक बजे बनिया पाँच रुपया देने वाला जो बरदानी शंख था, उसे रख दिया सिराहने पर झोले में और जो शंख ढपोर था उसे ले गया उठा करके। ब्राह्मण देख लिया जब शंख आ गया तो अपना झोला उठाया और चले। अपना तो काम बना। अब चार जब बजा, रात भर नींद न आई जी सेठ को अब उठाता है, सेठानी को। अरे, उठो न जी। क्या है? अरे, सो गई क्या बात है। अरे, उठो तो बतावें। उठा के बिठा दिया सेठानी को जाओ नहाओ, गाय के गोबर से चौका लगाओ और नई साड़ी पहन लो। अब सेठ और सेठानी नहा धो के नया कपड़ा पहनकरके दोनों गाँठ जोड़कर, शंख ढपोर को रख दिया आसन के ऊपर। पूजा-पाठ, धूप-दीप, नैवेद्य सब कुछ किया। अब सेठ कहता है, जय हो महाराज ! देव महाराज एक लाख रुपया। वो बेचारा गरीब था एक हजार मांगा। सेठ एक लाख से क्या कम मांगे। शंखढपोर कहता है- ले रे बनिया! दस लाख। मिला न एक पैसा। एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन इस तरह होता रहा तो आठ-दस दिन बाद सेठ कहता है रोकर के। महाराज कहते तो तुम बहुत हो देने को। जितना माँगता हूँ, उसका दस गुना देने को कहते हो, बोलते हो, मगर देते-लेते एक पैसा नहीं। तो शंखढपोर कहता है- बेवकूफ कहीं के ये देना-लेना जो है वो शंखिया का काम था। हम तो शंखढपोर हैं, कहते भर हैं, देना-लेना एक पैसा नहीं।
तो भैया ! भगवान आत्मा को छोड़कर और बाकी जितनी बातें सब शंखढपोरी है. सुनते बस रहो, तथ्य किसी में नहीं है। हाँ, ये बात और है कि हम खंडन किसी का नहीं करते। विरोध किसी का नहीं करते। आलोचना किसी की नहीं करते। ये सब चीज जितनी हैं, जो अपने आपको संसारी मानते हैं। इन अज्ञानी बालकों के लिए ये सब उनको समझाने के लिए कही गई है, क्योंकि सभी को विचार जगत में अधिकार नहीं है न। तो उनके लिए ये सब बातें ठीक हैं। परन्तु वास्तविकता अगर देखो भैया। तो जीव जगत में विचार की गुंजाइश नहीं है। आत्म जगत में विचार करो। किसी प्रकार से करो सिवाय मुझ आत्मा के अस्तित्ववान के, आत्मा के चराचर का अस्तित्व जो है, इसके सिवाय किसी में तथ्य नहीं। सब अफसाना है, कहानी है।
व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवेकेन गच्छति ।
यथातृणजलूकैवं देही कर्मगतिं गतः ।।
(10-1-40)
स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथे नाभि निविष्टचेतनः ।
दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृतिः ।।
(10-1-40)
देखो, दिन में जो कुछ भी देखा जाता है और सुना जाता है, क्योंकि संसार का प्रवेश हृदय में दो ही इन्द्रियो के द्वारा होता है-देख करके और सुन करके। क्योंकि, नाम, रूप ही संसार है। तो चक्षु और कर्ण दोनों इन्द्रियों के द्वारा हृदय में संसार प्रवेश करता है। तो दिन में जो कुछ भी देखा सुना जाता है। मन उन देखे-सुने का चिंतन करता है और चिंतन करते-करते जब सो जाता है। तो जिसके चिंतन में सोता है, उसी का स्वप्न देखता है।
स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथे नाभि निविष्टचेतनः ।
दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृतिः ।।
(10-1-41)
ये दृष्टांत है जो दिया हुआ है श्लोक में। अब इसका खास मतलब क्या है? अनादि काल से अज्ञान जगत में जीव जगत् में मान्यता जगत् में, कल्पना जगत् में सुन-सुन और देख-देखकर। क्या देखकर ! कि पुण्य कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा और पाप कर्म के करने से नर्क। ये कर्म करो तो इस लोक को जाओ और वो करो तो उस लोक को जाओ। देखो तो नहीं किसी ने अदृष्ट है न। अच्छा, सुन रहे हो ये संस्कार आज का नहीं है। अनादिकाल का है। ये पाप कर्म है, मैं कर रहा हूँ और मरने के बाद हमें नर्क जाना पड़ेगा। पुण्य और पाप हमें मरकर स्वर्ग-नरक जाना है-ये आज का संस्कार है, नहीं है। अनादिकाल का है। मेरा आना है, जाना है। दुःख है, सुख है। ज्ञान है, अज्ञान है। नर्की हूँ, स्वर्गी हूँ। धर्मी हूँ, अधर्मी हूँ इत्यादि ।
भैया, ये सुनते चले आ रहे हैं। इसका संस्कार हृदय में दृढ़ हो गया है। अब जब मरते हैं, माने शरीर जब छूटता है, तब मरने के बाद उसी का बादशा बिंच जाता है। अच्छा, उसी प्रकार से जैसे, अरे, जो नरक गया है, वहाँ से किसी ने आज तक टेलीग्राम नहीं किया और जो स्वर्ग गया है, वहाँ से किसी ने पत्र नहीं डाला। अपने बच्चों को कि बड़ी अच्छी सीट मिली है, चिंता- फिकर मत करना। तो अदृष्ट ही तो है न।
हम शास्त्र वाक्य पर विश्वास करते हैं, विद्वानों के कथन पर विश्वास करते हैं, आस्तिक होने के नाते, परन्तु यहाँ विचार की गुंजाइश नहीं है। जैसा सुनते हो, वैसा मानते हो और हृदय में इनके संस्कार पड़े हुए हैं। जब देह छूटती है, तब हमको वही अनादिकाल के जो संस्कार हैं, वही सब मरने के बाद दिखाई देता है। नरक दिखाई देता है, स्वर्ग दिखाई देता है और इतने दिन तक स्वर्ग में रहना पड़ता है। इतने दिन तक नरक में रहना पड़ता है, उसी तरह से भोग भी होता है। क्योंकि, जब मनुष्य सपना देखता है तो क्या उसको इस बात का ज्ञान रहता है कि जो मैं देख रहा हूँ, वो स्वप्न है? जागृत अवस्था की स्मृति उसे नहीं रहती और जागकर के मैं स्वप्न में आया हूँ, इसकी भी स्मृति नहीं रहती, उस स्वप्न दृष्टा को। उसी तरह से सुख भोगता है, दुःख भोगता है। उसी तरह से उसका परिवार बन जाता है। सब सारा संसार, दूसरा तैयार हो जाता है, स्वप्नावस्था में और जाग जब गया तो कुछ नहीं।
इसी तरह भैया, जीव का जो गमनागमन है, जीव का जो नाना योनि में जाना है, भटकना है। ये पुराने जो संस्कार हृदय में पड़े हैं। शरीर छूटने के बाद बिल्कुल वहीं का वही। इसलिए जीव का गमनागमन नरक स्वर्गादि का भोग स्वप्न है। मोह की नींद का स्वप्न है। गफलत की नींद का ख्वाब है।
अच्छा, ज्ञान होने पर मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब ये कि ज्ञान होने अच्छा, अब चलो मोक्ष पर विचार करते हैं। ज्ञान होने पर मोक्ष हो जाता पर गमनागमन से छुटकारा पा जाता है।
'ऋते ज्ञानं न मुक्ति' श्रुति भी कहती है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं तो जितने जीव मुक्त होते हैं, तो मुक्त होकर जाते कहाँ हैं? अरे, उनका कोई वेटिंग रूम बना है, जहाँ मुक्त जीव जाकर भड़भड़ा के भरे हुए हैं? कहाँ जाते हैं? किस लोक में जाते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? इसको भी सुनो। जीव का गमनागमन स्वप्न है, और जीव का मोक्ष सुषुप्तिवत्- जीव का गमनागमन स्वप्नवत् है-स्वप्नवत् । वत् प्रत्यय लगा देने से स्वप्न के समान। जीव का गमनागमन स्वप्नवत् (के समान) है और जीव का मोक्ष सुषुप्तिवत् है। जैसे- गाढ़ी निद्रा में प्रपंच का अभाव हो जाता है। संसार नहीं रहता, प्रपंच नहीं रहता मगर चेतन जो है, आत्मा। ज्यों का त्यों रह जाता है। मगर सुषुप्ति अवस्था में मैं कौन हूँ? मैं कहाँ था? मैं क्या होऊँगा। तीनों काल की स्मृति सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहती। इसी प्रकार, इसी तरह मोक्ष हो जाने पर सुषुप्ति के समान उस मुक्त जीव की स्थिति हो जाती है। जी हाँ! सुषुप्तिवत् ! यही वास्तविक है। जी हाँ ! तो 'स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं'। ये जीव जगत की बातें बताई जा रही हैं। अध्यात्म जगत में तो कुछ है ही नहीं।
यतो यतो धावति दैवचोदितं मनो विकारात्मकमाप पञ्चसु ।
गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ।।
(10 - 1 - 42)
ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेष्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते ।
एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ।।
(10 - 1 - 43)
जैसे किसी पात्र में पानी भरकर रख दो, जैसे-टब आदि तो उसमें सूर्य दिखाई देगा। अब हवा चलने से जब उस टब का पानी हिलेगा तो पानी हिलने से सूर्य भी हिलता दिखाई देगा। मगर ऐसा है नहीं। सूर्य तो ज्यों का त्यों अपने स्थान पर है। इसी तरह वासना रूपी हवा के झकोरे से जब अन्तःकरण चंचल होता है या मन चंचल होता है या बुद्धि चंचल होती है तब उस चंचलता को अज्ञानी अपने स्वरूप में मानता है कि मैं आता-जाता हूँ। देखो, अन्तःकरण है त्रिगुणात्मक। हरेक के अन्तःकरण में तीन गुण रहते हैं। मन कह लो या अंतःकरण। तो मन में कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी और कभी तमोगुणी। तो मन के सात्विक, राजस, तामस ये तीनों विकार हैं। समय-समय पर अज्ञानी को ये विकार दिखाई देते हैं, तो मानता है, ये विकार मेरे हैं। मगर ऐसा नहीं है।
मानसकार कहते हैं-
बालक भ्रमहिं न भ्रमहि गृहादि। कहहिं परस्पर मिथ्यावादी ।।
चार-छह बच्चे आठ-दस साल के आपस में इकट्ठे होकर हाथ में हाथ मिलाकर चक्कर घूमते हैं। यहाँ इस प्रान्त में इसको 'घानीमुनी' कहते हैं और उत्तरप्रदेश की भाषा में 'घुमरी परैया' कहते हैं-अच्छा, अब वो 'घानीमूनी' के खेल में घूमते-घूमते चक्कर आ जाता है बच्चे को और गिर जाता है। तो उसको दुनियाँ क्या दिखाई देती है? कि मेरे समेत सारा संसार घूम रहा है। मगर मानसकार कहते हैं कि न तो वो बच्चा घूम रहा है और न ही घर-द्वार, संसार। उस चक्कर के कारण उसको ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा मालूम होता है। इसी तरह अज्ञान का ऐसा चक्कर है। तो इस चक्कर की वजह से अज्ञानी जीव क्या मानता है? जिस तरह मेरा आवागमन है। जिस तरह नाना योनियों में मैं आता- जाता हूँ, इसी प्रकार मेरे समान सारे संसार का आवागमन है। जी हाँ, चक्कर जब शांत हो जाता है, अज्ञान जब निकल जाता है, विनाश हो जाता है। तब जिस तरह मुझ आत्मा का आवागमन नहीं, मैं आत्मा अजर-अमर-अविनाशी व्यापक तत्व। अरे, इसी तरह किसी का आवागमन, बिल्कुल नहीं। मेरा आवागमन है तो दुनियाँ का है और मेरा आवागमन नहीं तो किसी का नहीं। ये अपने ही निश्चय से, सबका निश्चय होता है। अपने ही अनुभव से सबका अनुभव होता है। अपने ही ज्ञान से सबका ज्ञान होता है। तो-
ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेष्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते ।
एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ।।
(10-1-43)
तो महात्मा वसुदेव कंस को समझाते हैं- भैया ! इसीलिए किसी से द्रोह मत करो, देवकी को मत मारो। बहुतेरा समझाया तो सही, मगर कंस कहता है-मैं तो मार ही डालूंगा।
वसुदेव जी ने सोचा इस दुष्ट के हाथों से देवकी का प्राण बचाना अच्छा है । तो तुम ऐसा करो यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे लिए तो आकाशवाणी आठवें गर्भ के लिए हुई है परन्तु मैं प्रतिज्ञा करता है कि पहला ही बालक जो होगा, उसे नाल सहित मैं तुम्हारे है। पास ले आऊंगा। मार डालना या रक्षा करना ये सब तुम्हारे ऊपर है। अब इसे छोड़ दो तो कंस ने कहा-अच्छी बात है, मैं प्रसन्न हूँ, ले जाओ। अब दम्पत्ति अपने स्थान को आये। जैसे ही पहले बालक का जन्म हुआ महात्मा वसुदेव उसे ले जाकर रख दिये कंस के सामने, क्योंकि सत्य प्रतिज्ञ थे, सत्यनिष्ठ थे। तो कहते हैं-
किं दुःसहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम् ।
किम कार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं कि धृतात्मनाम् ।।
(10 - 1 - 58 )
'साधूनां किं दुःसहं ।' अरे जो साधु लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, संसार में ऐसा कौन सा दुःख है जिसे सहन न कर सके, सब सहन कर लेते हैं। और जो विद्वान हैं वो किसकी उपेक्षा नहीं करते और जो कदर्य नीच हैं, महान दुष्ट हृदय हैं, कौन-सा बुरा से बुरा काम है, संसार में उसे न कर डालें और जो धैर्यधारी हैं, वे कौन-सा ऐसा पदार्थ है जिसका त्याग न कर सके। जब कीर्तिमान नाम के पुत्र को वसुदेव जी रख दिये, कंस के सामने तो देखते ही कंस प्रसन्न हो गया और कहता है-
प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम् ।
अष्टमाद् युवयोर्गर्भान्मृत्युर्मे विहितः किल ।।
(10 - 1 - 60)
वसुदेव जी ! भैया ले जाओ इसे तुम तो बड़े महात्मा निकले। हमें क्या पता था, तुम बड़े महात्मा हो, सत्यवादी हो, ले जाओ इसे। मेरे लिए जो आकाशवाणी हुई है, वह आठवें गर्भ के लिए है। ये तो पहला ही बच्चा है, उससे मुझे कोई भय नहीं। अब वसुदेव जी वापस ले आये।
जब वसुदेव जी वापस ले आये, वध न किया कंस ने उसका तो देवताओं के पेट में मरोड़ शुरू हो गया। अपना-अपना पेट पकड़े बैठे हैं सब।
नारायाण ! नारायण ! नारदजी आईये गुरुदेव ! आया देवराज ! - देवलोक में आनंद मंगल है न? आज तुम देवता किस गोष्ठी में बैठे हो, क्या विचार कर रहे हो? गुरुदेव ! आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको तो पता ही है कि देवकी के गर्भ से पहला बच्चा हुआ है। नारायण। नारायण। हुआ है तो तुम्हें क्या इससे-बात ये है कि आपने ये भी सुना है न कि जब तक देवकी के आठों पुत्रों का वध कंस न कर देगा तब तक सरकारी टूर होगा ही नहीं यानि अवतार ही नहीं होगा। बस ! अब बाबा वहाँ से वीणा बिनबिनाते पहुँचे मथुरा। दरबार लगा है-नारायण ! नारायण ! दौड़ा कंस दण्डवत् प्रणाम किया-भोजराज ! महाराज । प्रजा मंडल सुखी है न?-कृपा है महाराज। गुरु महाराज आज कैसे आना हुआ। अरे भाई-कुछ खास बात बताने ही आये हैं और पूछने भी आये हैं। तुम तो जानते ही हो कि पृथ्वी मंडल पर महापुरुषों का परिभ्रमण जीवों के कल्याण के निमित्त ही हुआ करता है।
मैंने सुना है कि देवकी के गर्भ से कोई पुत्र हुआ है। हाँ महाराज, हुआ तो है। गुरुदेव ! क्या किया फिर तुमने, कुछ नहीं वसुदेवजी लाये तो थे। मैंने वध नहीं किया, क्योंकि देवकी का आठवाँ गर्भ मेरा काल है। आकाशवाणी तो ऐसी ही हुई है। तेरे जैसे-उद्ध-बुद्ध, राजे-महाराजे आकाशवाणी का मतलब लगाने लगे तो हम साधु को कौन पूछे ? अब इतना कहने की देरी थी कि कंस सुकुड़दुम हो गया। बताओ महाराज आकाशवाणी का क्या अर्थ है? अच्छा बोल क्या हुई आकाशवाणी-
अष्टमाद् युवयोर्गर्भान्मृत्युर्मे विहितः किल ।।
(10-1-60)
देवकी का आठवाँ गर्भ जो होगा वो तुम्हारा काल पैदा होगा। बस ! यही अर्थ लगाया तूने। कौन-सा आठवाँ शुरू का, कि आखिरी का, कि बीच का? कौन-सा आठवाँ ? एक गोल सर्कल बनाया आकार में आठ रेखाएं खींच दिया। ले तू गिनती कर अब एक, दो, तीन... ले यहाँ से गिन..... गोल में जहाँ से गिन आठ ही आता है। अगर यही आठवाँ हो तो? जय हो महाराज, बड़ी कृपा करी महाराज-देवताओं का काम बना बाबा तो चले। अब उस पुत्र (कीर्तिमान) को बुलवाकर वध किया और उसी प्रकार देवकी के छह पुत्रों का नाश किया कंस ने। अब सातवीं बार भगवान वल्देव आये गर्भ में तब भगवान ने योगमाया को बुलाया अकेले में, और कहा-देवि !
गच्छदेवि ब्रजं भद्रे गोपगोभिरलंकृतम् ।
रोहिणी वसुदेवस्य भार्याऽऽस्ते नन्दगोकुले ।
अन्याश्च कंस संविग्ना विवरेषु वसन्ति हि ।।
(10 - 2 - 7)
देखो, सरकारी काम आ गया है- 'महाराज, आज्ञा।' आज्ञा यही है देवकी के गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में ठहराओ। देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा और बाबा नन्दजी की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम्हारा जन्म होना चाहिए। अब जाओ, तुम डरो मत। कालिकाल में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी।
नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि ।
दुर्गेति, भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च ।।
(10-2-11)
कुमुदा चाण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च ।
माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ।।
( 10- 2 - 12 )
तमाम तुम्हारे नाम रखे जायेंगे। धूप, दीप, नैवेद्य से बड़ी भारी पूजा होगी तुम्हारी कलियुग में। इतने पर भी योगमाया ने स्वीकार न की तब। अरे, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। तुम घबराती काहे को हो। कलियुग में जाओ, मेरा वरदान है, भारत की प्रधानमंत्री बनोगी। तो प्रधानमंत्री के लालच में योगमाया ने भगवान की बात मान ली। अरे, मामूली वरदान है, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री होना कोई मजाक है। मखौल समझे हो। बस ! महारानी आयी योगमाया। ये कोई मजाक की बात नहीं, जितनी बैठी हैं, सब योगमाया हैं। अरे, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर।
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो तोऽखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ।।
(श्री दु.सप्त. अ. 11/3)
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सुं ।
त्वयैकया पूरितमम्ब यै तत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ।।
(श्री दु.सप्तअ. 11/6)
या देवी सर्व भूतेषु स्त्री रूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।।
तो साक्षात् देवी तो हैं। जी हाँ। इनके एक हाथ में स्याही और एक हाथ में सफेदी। जी हाँ। ये किसी को चाहे आसमान में चढ़ा दें, चाहे पाताल में धँसा दें सब कुछ इनके हाथ में। इसलिए- 'इन्हहिं विरोधे नहिं कल्याना।' हाँ प्रसन्न, रखा करो भैया, जिनके जिनके यहाँ योगमाया हैं। देख लेना कल से हमारा नेवता शुरू हो जायेगा।
हाँ, एक दफे बड़ोदा गये बारह तेरह बरस की बात है। काठियावाड़ गुजरात में, बड़ोदा में, हमारी कथा हुई। गीता पर हो रहा था प्रवचन दो माह रहे, चातुर्मास किये थे। शाम को कथा होती थी। दो घंटा प्रवचन हुआ करता था। कई दफा ऐसा मौका आ जाता है, कहने को तो वहाँ पर, यहाँ पर जो शहरों में द्विजटा होती है-दो गुत्थियाँ बांधती हैं, लड़कियाँ। वहाँ पर त्रिजटा देखा। वहाँ पर कॉलेज की लड़कियों की तीन-तीन जटायें देखी तो त्रिजटा नाम रखा है मैंने। अब आ गया भाई ऐसा कोई प्रसंग कथा में तो हमने फैशन के ऊपर कुछ बोल दिया, भैया।
'त्रिजटा नाम राक्षसी एका' - और कोई फैशन के ऊपर। सेंडिल के ऊपर वहाँ सब लड़कियाँ बेल्ट बांधती हैं। कमर पतली करने के लिए वहाँ का फैशन अलग किस्म का है।
लो भैया ! दूसरे दिन से हमरा नेवता बंद हो गया। चार-पाँच दिन अपने पास से खाना पड़ा हमको। अब ये पता न लगे। श्रोता तो सब आते हैं। ये क्या कारण है कि नेवता बंद हो गया? इतना लम्बा-चौड़ा खर्रा कॉलेज की लड़कियों ने लिखकर भेजा हमको। उसमें लड़कियों ने एक बात लिखी - 'स्वामी जी आपने जो आलोचना की है, फैशन के ऊपर, जो चीज व्यापक होती है, दोष नहीं मानी जाती ।' - बात तो सही है, वाजिब है। दोष उसको कहते हैं, जो कुछ में हो और कुछ में न हो। मगर जहाँ कहीं आप जायेंगे, बाम्बे जायेंगे, कलकत्ता जायेंगे, लाहौर चाहे कहीं भी-संसार भर में आप देखो। क्या देश- विदेश तो इसी तरह का फैशन देखेंगे। ये दोष नहीं है। हाँ, लिहाजा आपने जो कहा है, आप तो महात्मा हैं, विद्वान हो क्या कहें। अरे! हम समझ गये। मैंने कहा अब पैंतरा बदलना चाहिये।
पाँच-सात साधु और थे साथ में, रोज अपने पास से भैया, खर्च करके छाया करें। दूसरे दिन, फिर हमने ऐसा प्रसंग लाया कथा में, ऐसी लम्बी-चौड़ी महिमा गाई हमने, देवियों, धन्य हो, धन्य हो, सनातन धर्म की नींव तुम्हारे हाथ में है। हाँ, ये देवियाँ अगर दान-पुण्य न करें, ये कुछ न करें तो साधु भूखे मर जायेंगे। जो महिमा गायी हमने दो घंटे, फिर तो धड़ाधड़ नेवता। इसलिए भैया महामाया हैं।
हाँ जी ! अब योगमाया आयीं और आ करके उस गर्भ को खींचकर के रोहिणी के गर्भ में ठहरायी इसीलिए भगवान बलरामजी का नाम 'संकर्षण' पड़ा। क्योंकि, आकर्षण किये गये हैं न।
गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया ।
अहो बिस्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुकुशुः ।।
(10-2-15)
मथुरापुर वासियों एवं कंस को ये निश्चय हो गया कि छह पुत्रों का वध तो हो ही गया है। सातवाँ पुत्र जो है देवकी का गिर गया, नष्ट हो गया। इस लीला का पता किसी को न लगा अब आठवीं बार भगवान कृष्ण आये गर्भ में-
ततो जगन्मङ्गल मच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी ।
दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः ।।
(10 - 2 - 18)
अरे भाई, पता है कंस को कि छह पुत्रों का वध हमने कर दिया और सातवाँ गिर गया। जैसा कि अनुमान है आठवाँ यही है, जिसके लिए आकाशवाणी हुई है। परंतु कंस का जानना न जानने के समान है। भैया, ये 'खल ज्ञान' है इसको खल ज्ञान कहते हैं।
आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीम् ।
चिन्तयानोहृषीकेशम पश्यत् तन्मयं जगत् ।।
(24-2-10)
चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते जागते सारा संसार कंस को भगवान हृषिकेश दिखने लगा। भय के कारण भोजन करते थाल में वही नजर आता है। थाल उठाकर फेंक देता है। बिस्तर पर से उठकर के भागता है। कंस की ये हालत हो गई। अब भगवान के अवतार लेने का समय आया तो ब्रह्मादिक देवता अर्द्ध रात्रि के समय कारावास में आते हैं और आ करके भगवान की गर्भस्तुति करते हैं।
सुनो अब, यहाँ सत्य का प्रतिपादन होगा जो जहाँ पर बैठे हो आनन्द लो- 'देवः उचुः' -
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये ।
सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ।।
(10-2-27)
'वयं देवाः त्वां स्त्यात्मकं शरणं प्रपद्ये'- भगवन् हम सब देवता जो हैं आपकी शरण में आये हैं। हे सत्यव्रत, हे सत्यमूर्ते आदि।
देखो, ये आत्मजिज्ञासुओं ! भैया, अब पहले सत्य पर विचार करें, सत्य क्या होता है। 'त्रिकालाबाध्यत्वं सत्यं'- क्योंकि श्रुतियाँ भी कहती हैं-सत्यं ज्ञान....... सत्यं शिवम् सुंदरम्। ज्ञान सत्य है, सत्यं आनन्दम्, ब्रह्म इत्यादि। तो परमात्मा सत्य कहा जाता है। देखो, त्रिकाला बाध्यत्वं सत्यं। जो पदार्थ त्रिकाला बाध्य होता है। माने जो पदार्थ तीनों अवस्था, तीनों काल में रहे, जिसका नाश तीनों काल में न हो जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में रहे, तीनों काल में जिसका कभी नाश नहीं होता। जो एक रस रहता है, उसको सत्य कहते हैं। अच्छा जो सत्य होता है, तो यह नियम है कि वो परिच्छिन्न माने लिमिटेड नहीं होता, व्यापक होता है, असीमित होता है। जो सत्य होता है, वो व्यापक होता है और जो व्यापक होता है, वो निरअवयव माने आकार-प्रकार उसका कुछ नहीं होता। जो निरअवयव होता है, वो निरंश होता है, जो निरंश होता है, वो अखंड होता है, वो अनन्त होता है। जो अनन्त होता है वो अद्वैत होता है, जो अद्वैत होता है, वो अजन्मा होता है, वो अमर होता है। जो अमर होता है वो अविनाशी होता है और सर्व का आधार होता है।
अच्छा, एक विशेषण समझ लेने पर भगवान के सब विशेषण सत्य के अपने आप आ जाते हैं। परन्तु ये नियम जरूर है, माने ये विधान, ये अटल सिद्धांत जरूर समझ लेना चाहिए कि सत्य पदार्थ का नियम है कि वो व्यापक ही होता है, वो सीमित नहीं होता, एक देशीय नहीं होता, व्यापक होता है। जी हाँ और जो पदार्थ व्यापक होता है, वह अक्रिय होता है, निरअवयव होता है, निरंश होता है। वो निरंजन होता है, निरअवयव होता है और निर्विकार होता है। ये नियम है और सत्य का यही अर्थ होगा। यहाँ सुनो या विश्व में कहीं चले बानो। जी हाँ, सत्य की परिभाणा यही होगी।
अच्छा सुनो! 'त्रिकाला बाध्यत्वं सत्यम्।' दूसरा नियम यह है कि जो पदार्थ सत्य होता है, वो स्वतः प्रमाण होता है, परतः प्रमाण नहीं होता भैया! स्वतः प्रमाण किसको कहते हैं? परतः प्रमाण किसको कहते हैं?
अभी हम इसको अच्छी तरह समझायेंगे। जिसका प्रमाण स्वयं हो वह स्वतः प्रमाण है और जिसका प्रमाता दूसरा हो परतः प्रमाण है। प्रमाता किसको कहते हैं? प्रमाता उसको कहते हैं, जो प्रमाणित करता है। जैसे- अब हमारे हाथ में डंडा है और तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछता है, पिताजी, स्वामीजी के हाथ में क्या है ये? तो तुम बताओगे कि भैया, स्वामीजी के हाथ में डण्डा है। तो तुम इस डण्डे के हुए प्रमाता। जो प्रमाणित करे उसको कहते हैं प्रमाता और डण्डा हुआ प्रमेय अर्थात् जो प्रमाणित किया जाये। तो प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। अब ये त्रिपुटी बन गई तीन प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय अच्छा, अब समझो जो सत्य होता है। अच्छा, ये भी नियम है कि प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये एक- दूसरे से अलग होते हैं। तो सत्य का प्रमाता जब सत्य को प्रमाणित करने आयेगा तो भाई सत्य से भिन्न होकर ही तो सत्य को प्रमाणित करेगा। जबकि प्रमाता प्रमेय से अलग है। और सत्य से जो भिन्न होगा, वह सत्य न होगा, असत्य होगा। तो असत्य में क्या ताकत है कि सत्य को प्रमाणित कर सके।
जो पदार्थ सत्य होता है, उसका अन्य प्रमाता नहीं होता और जो अन्य प्रमाण से सिद्ध होता है वो सत्य नहीं है। ये निर्विवाद सिद्धांत है। जी हाँ! इसलिए सत्य स्वतः प्रमाण होता है, परतः प्रमाण नहीं होता। जिसका प्रमाता कोई और होता है वो पदार्थ कालान्तर में नाश हो जाता है। तो देखो जो सत्य है, परमात्मा है, सबका अस्तित्व है, इसके अतिरिक्त जितने हैं वो परतः प्रमाण हैं। सत्य ही ऐसा है जो स्वतः प्रमाण है। सत्य का प्रमाता सत्य ही होगा और बाकी जो है, परतः प्रमाण है, अन्य करके प्रमाणित होते हैं। इसलिए कालान्तर में नाशवान माने जाते हैं। सत्य स्वसंवेद्य होता है, पर संवेद्य नहीं। स्वसंवेद्य का मतलब होता है कि सत्य का ज्ञाता सत्य ही होता है, सत्य को सत्य ही जानता है, अगर सत्य का जानने वाला सत्य से भिन्न है तो फिर वही आपत्ति आयेगी। असत्य, सत्य से भिन्न असत्य तो असत्य सत्य को क्या जानेगा? इसीलिए सत्य का परिज्ञाता सत्य ही होता है। इसलिए सत्य को स्वयंवेद्य कहते हैं, परसंवेद्य वहीं। सत्य स्वसंवेद्य होता है. परसंवेद्य नहीं। सत्य स्वतः प्रमाण होता है. परत: प्रमाण नहीं।
सत्य अहंगम्य होता है. इदंगम्य नहीं। देखो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक अहंगम्य और दूसरा इदंगम्य । चीजों का अनुभव यह लगाकर किया जाय, वह इदं गम्य है और जिसका अनुभव अहं भाव में हो वो अहंगम्य है। तो भैया, सत्य परमात्मा अहंगम्य है. दिगम्य नहीं। क्योंकि, इदंगम्य जो पदार्थ है, उसका नाश कालांतर में हो जाता है। तो परमात्मा का अनुभव यदि इदं भाव से मानोगे। परमात्मा को भी आता इदं वाच्य मानोगे तो कालांतर में उसका भी नाश हो जायेगा। केनोपनिषद की । इदम् माने यह और अहं माने मैं। जिन-जिन कुछ श्रुतियाँ आयी हैं, इनको सुन लो, फिर इनकी अनुभूति करायेंगे
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।।
(के.उ. 1-4)
वाणी जिसको व्यक्त नहीं कर सकती, वाणी को जो व्यक्त करता है तो श्रुति यहाँ प्रेस करती है, जोर देती है 'तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि।' अरे, उसको ही तू सनातन ब्रह्म जान। 'इदं रूपं यद उपासते तन्न।' इदं रूप से जिसकी उपासना की जाती है, वह परमात्मा नहीं है।
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।। 5 ।।
मन जहाँ नहीं जाता, मन जिसको नहीं जान सकता। मन को जो जानता है- 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं इति उपासते।' उसी को तुम सनातन ब्रह्म जानो। इदं रूप से जिसकी उपासना होती वह परमात्मा नहीं है।
यच्छ्रोत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद मुपासते ।।
(के.उ. 1-7)
कर्ण इन्द्रिय द्वारा जो गोचर नहीं। कर्ण इन्द्रिय द्वारा जो नहीं सुना जाता। करे. कान के सुनने न सुनने को जो सुनता है, वही सनातन ब्रह्म है, वही पामात्मा है, वही सत्य है। वही स्वस्वरूप भगवान आत्मा है।
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद मुपासते ।।
( के.उ. 1-8)
प्राण जिसको संचारित नहीं कर सकता, प्राण को जो संचारित करता है 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं इति उपासते।' उसी को तुम सनातन ब्रह्म जानो। भैया, श्रुतियाँ इस प्रकार ललकार रही हैं। इस तरह से प्रमाणित कर रही हैं। जी हाँ! जो सत्य है, जो परमात्मा है, वो इदं वाच्य नहीं है, क्योंकि इदं गम्य यदि मानोगे तो नाशवान है। और यदि अहं गम्य जानोगे तो प्रतिपादन तो इसका रात-दिन हो ही रहा है। इसमें क्या बड़ी भारी बात है। तो अहं रूप से मैं रूप से परमात्मा की अनुभूति होती है। परमात्मा जाना जाता है, उसका दर्शन होता है, इदं रूप से नहीं।
ईश्वर का अनुभव अगर तुम इदं रूप से मानते हो तो कालांतर में इसका नाश हो जायेगा, नष्ट हो जायेगा ईश्वर। और अहं भाव से अगर जानते हो, अहंगम्य अगर जानते हो तो फिर अहमेव इसका तो प्रतिपादन हो ही रहा है। समझो इस चीज को तो सत्य स्वतः प्रमाण होता है, परतः प्रमाण नहीं, स्वसंवेद्य होता है। परसंवेद्य नहीं। अहंगम्य होता है, इदंगम्य नहीं। जी हाँ! देखो, वेद, शास्त्र, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, रामायण, भागवत, संत-महात्मा तथा हम स्वयं हमारा अनुभव। जी हाँ! यही है कि सारे चराचर में जो व्याप्त है, सर्व का जो अस्तित्व है और हरेक के अंदर मैं हूँ, मैं हूँ, रात-दिन जो कह रहा है, रट रहा है, पुकार रहा है। हाज़िर-नाज़िर है। जाहिर-जहूर अभिव्यक्ति हो रही है। सबके अंदर से जो प्रस्फुटित हो रहा है। सब में जो प्रस्फुरित हो रहा है, वो भगवान ही है। वही भगवान आत्मा है, वही सत्य है, वही सनातन है, वही व्यापक है।
प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्धबोधस्वभावः
सदसदिदमशेषं भासयन्निर्विशेषः ।
विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्व वस्था-
स्वह महमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः ।।
(वि.चू.म. 137)
'प्रकृति विकृति भिन्नः' जो परमात्मा प्रकृति-विकृति से भिन्न है। प्रकृति माने कारण और विकृति माने कार्य। परमात्मा न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। न उससे कुछ पैदा हुआ और न वह किसी से पैदा हुआ। शुद्ध बोधस्वभावः, शुद्ध बोधस्वभाव है। मैं अमुक हूँ, यह अशुद्ध बोध है और मैं हूँ, यह शुद्ध बोध है और सत असत से परे है।
जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था तीनों अवस्थाओं के प्रपंच में जो विलास करता है। जाग्रत अवस्था के प्रपंच को कौन जान रहा है कि ये पुरुष समाज है, ये प्रकृति समाज है। ये प्रकाश है, ये अंधकार है। उसको कौन देख रहा है? कौन जान रहा है? कौन अनुभव कर रहा है। तो 'विलसति परमात्मा जाग्रदा दिष्ववस्था स्वह महमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः।' और हर एक के अंदर स्वह महमिति-अहम इति, अहम इति मैं हूँ, मैं हूँ ऐसा जो परमात्मा अपने आपको जाहिर कर रहा है, बयान कर रहा है। अपने आपको व्यक्त कर रहा है। तो किसी प्रकार से समझ लो युक्तियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा दृष्टांतों के द्वारा, स्वानुभव के द्वारा। जी हाँ। परन्तु आश्चर्य कि ये सब होने के बावजूद दो अकल की कमी के कारण बात दिमाग में नहीं बैठती। अब दो दो अकल का दृष्टांत आ गया है, सामने वह कह रहा है हमें सुनाकर फिर चलो।
देखो भैया ! एक दृष्टांत है दो अकल की कमी का। एक राजा था। उस राजा की एक राजकुमारी थी, एक कन्या थी। जब वो सयानी हो गई, शादी के काबिल, तो राजा ने कर्मचारियों को बुलाकर कहा भैया, राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर ढूँढ़ो। अच्छा हृष्ट-पुष्ट हो, सुंदर हो, राजकुमारी के योग्य हो, रियासत, इस्टेट अच्छी हो। जब कर्मचारी वर ढूँढ़ने जाने लगे और राजकुमारी को पता चला कि हमारे पिता राजा-महाराज हमारे लिए वर ढूँढ़ने कर्मचारियों को भेज रहे हैं, तो राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि पिताजी-हमने ऐसी-ऐसी बात सुनी है। राजा कहते हैं-हाँ बेटी! क्या विचार है, शादी नहीं करेगी क्या? नहीं, शादी तो मैं करूँगी। मगर एक शर्त है। शर्त ये है कि जिस राजकुमार में पूरी सौ अकल होगी, उस राजकुमार से ब्याह करूँगी। राजा ने कर्मचारियों से कहा देखो, भाई रियासत तो देखोगे ही, राजकुमार भी देखोगे मगर ये पूछ लेना पहले कि तुममें कितनी अकल है।
कर्मचारियों ने कहा-जो आज्ञा ! अब जायें तो राजकुमार देखे, सुंदर रियासत, स्टेट सब कुछ और पूछें भाई तुममें कितनी अकल है? तो कोई राजकुमार कहे हममें पचास है, कोई कहे पैंसठ है। याने वर्षों ढूँढ़े पर साठ-पैंसठ से ज्यादा अकल वाला कोई मिला ही नहीं। परेशान हो गया राजा भी। बेटी! पचास- साठ अकल से ज्यादा कोई मिलता ही नहीं। अब तू कहे तो राजकुमार न ढूँढ़ कर कोई जाति का वर ढूँढ़ लें, क्योंकि अन्तर्जातिय विवाह तो चालू ही है। पिताजी कोई हर्ज नहीं है कर लूंगी मैं ब्याह, बशर्ते की सौ अकल हो।
अब कर्मचारी चले ढूँढ़ने और तो कोई न मिला। एक भैंस चराने वाला, अच्छा तेंदू का डंडा, काला-काला रखे कंधे पर, पगड़ी बांधे बैठा है, भैंस चर रही है। पच्चीस साल का जवान पट्ठा, भैंस का दूध पी के करिया भुसुंड।
कर्मचारियों ने सोचा कि चलो सगुन तो अच्छा है। इसी से पूछें-क्यों भैया, तेरा क्या नाम है। मेरा नाम पुसऊ ! कहाँ रहता है, बोले-रायपुर। क्या करता है? देखते नहीं, सब भैंसें चर रही हैं। तेरे माँ-बाप हैं? सब हैं। शादी करेगा? उसने कहा तैयार ही बैठे हैं। तेरे पास कितनी अकल है? उसने ललकार के कहा अन्ट्ठानबे। नब्बे, आठ अन्ठानबे अकल है। तब ठंडी सांस लिया कर्मचारियों ने कि चलो मुद्दतों के बाद अन्ठानबे अकल वाला कोई मिला। जात-पाँत का तो परहेज कोई रहा नहीं। पक्का करके आ गया। राजकुमारी को राजा ने बुलाया- बेटी और तो कोई मिला नहीं। एक भैंस चराने वाला मिला है पहाटिया अहीर है, अन्ठानबे अकल वाला है। करेगी शादी? तैयार हूँ, दो ही कमी है न? मैं सिखा लूंगी। अब शादी पक्की हो गई। बाजा-बजा। पुसऊ महाराज का ब्याह हो गया। अब, जब रनिवास पुसऊ पहुंचे। कहाँ रानी राजकुमारी और कहाँ पुसऊ। बेतुका हिसाब । राजकुमारी जाकर अभिवादन करती है। तो पुसऊ कहते हैं-राम-राम। राजकुमारी कहती है कि आप तो हमारे पति हो न? इसमें भी अभी शक है क्या? क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आपके अंदर कितनी अकल है? पुसऊ ने कहा कि अन्ठानबे। क्या आप बता सकते हैं वो दो अकल कौन-सी नहीं है, आपके अंदर। अन्ठानबे तो हैं ही, मगर वो दो अकल नहीं है, वो कौन-सी नहीं है, दो अकल। पुसऊ कहते हैं कि-एक अकल तो ये नहीं है कि मैं कुछ जानूँ नहीं, ये पहली अकल है। और दूसरी अकल ये नहीं है कि किसी की कुछ मानूँ नहीं।
परेशानी है दादा मत्था फोड़ रहे हैं रोज। आज पूरे चार दिन हो गये। धड़ाधड़ प्रतिपादन, ब्रह्म निरूपण हो रहा है। सबको अनुभूतियाँ रोज करा रहे हैं। रामायण, गीता, भागवत, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, वैदिक मंत्र, सबका प्रमाण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, युक्तियाँ दे रहे हैं। स्वानुभव बता रहे हैं। मगर।
अरे भाई सद् शास्त्रों को देखा नहीं, विद्वान संत, महात्माओं का सत्संग किया नहीं। कभी विद्वानों, महापुरुषों की गोष्ठी में गये नहीं। संत समाज देखा ही नहीं। न तो मैं कुछ जानता हूँ और कोई भूले-भटके अगर बताने वाले आ भी जाते हैं तो फिर मानूँ नहीं। भला ये नाव दरिया कैसे पार होगी। किनारे लगेगी कैसे अरे, विद्वान हो तो शास्त्रों का प्रमाण लो ललकार के। अगर विद्वान हो तो वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक शास्त्रों का प्रमाण लो और नहीं पढ़े हो तो युक्तियों का प्रमाण लो। यदि श्रद्धालु हो तो संत वाक्य का प्रमाण लो। किस बात का? शरीर से परे, शरीर से भिन्न शरीर के अंदर जो व्यापक सच्चिदानंद घनभूत । शरीर के अंदर व्यापक, शरीर से परे जो 'मैं' चेतन तत्व आत्मा इससे जो भिन्न है वो परमात्मा नहीं। बस ! इसको चाहे अभी समझ लो या लाखों जन्म के बाद। मगर याद रखो, यारों इसके बिना समझे तुम्हें सुख और शांति नहीं है। जी हाँ! अगर हम प्रतिज्ञा करते हों तो प्रतिज्ञा वाक्य पर विश्वास न करो। मगर वेदों पर, रामायण, गीता भागवत पर अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो इसका प्रमाण दिया जा रहा है। ये सिद्धांत कोई मजहबी सिद्धांत नहीं है। कोई पंथ-पंथाई या सोसायटी का नहीं है। ये अध्यात्म तत्व है। ये सर्व का अपना आप है। व्यापक सिद्धांत है।
भगवान आत्मा ही एक ऐसा पदार्थ है जो प्रेक्टिकल है। अनुभव करने में आ सकता है। बाकी सब कहानी है। अरे, बाप दादों के जमाने से सुनते चले आ रहे हो कि ईश्वर है। परमात्मा है। मगर, अब तो देखने का जमाना है। कब तक अंधेरे में रहोगे। उजाले में रहना भी तो सीखो। अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवों उठो ! जागो, अपने स्वरूप में और देखो तो मैं कौन हूँ? परमात्मा किसे कहते हैं। विचार करो। ये कोई किताबी चीज नहीं है, अनुभव की चीज है न। आज कोई नास्तिक आता है तुम्हारे सामने और कहता है कि क्या ईश्वर है? तो ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण है। सारे विश्व के विद्वानों से ये प्रश्न है कि ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण है? शास्त्र दिखाओगे?
ईश्वर के अस्तित्व में 'मैं' आत्मा ही प्रमाण हूँ। जब तुमसे कोई पूछे ईश्वर है? तो अकड़कर कहना - हाँ! क्या प्रमाण है पूछे तो कहना कि मैं हूँ इसलिए ईश्वर भी है और मैं आत्मा नहीं तो ईश्वर भी नहीं। 'अहं' करके ईश्वर की सिद्धि होती है। 'मैं' करके, आत्मा करके न कि शास्त्र और वेद करके। जबकि वो मन, वाणी का विषय नहीं। भगवान कहाँ है, जहाँ मैं हूँ। मैं कहाँ हूँ? जहाँ भगवान है। भगवान कौन है, जो मैं हूँ। मैं कौन हूँ? जो भगवान है। ये निर्विवाद सिद्धांत है बिल्कुल।
सत्यव्रतं सत्य परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये ।
सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ।।
(10 - 2 - 27)
'जैसे बहे बयार पीठ पुनि तैसे दीजै।' यार! रोटी चुपड़ी अच्छी लगती है, मगर बात चुपड़ी नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट कहना चाहिए। जी हाँ! वही बात कही जायेगी जो तुम्हारे कल्याण की होगी। जो तुमको अच्छी लगेगी, वो न कहूँगा मैं।
सचिव वैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस ।
राज धर्म तन तीनि कर होहिं बेगिहीं नास ।।
(राम.मा.सु.कां.दो. क्र. 37)
कुदरत ने हमें गुरु पद पर बैठाया है तो मैं वही कहूँगा जो तुम्हारे लिए हो, जिससे तुम्हारे चित्त को शांति मिले। क्योंकि मरीज जो है, रोगी जो है, कुपथ मांगता है।
कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी। बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ।।
ये तुम्हारे कल्याण की बातें कही जा रही हैं। कथा भाग मैं बिल्कुल कम कहता हूँ। जब टाइम रहा। याद रहा तब कुछ कह देता हूँ। क्योंकि ये कथाएँ तो संसारी विद्वानों, कथा वाचकों से भी भैया तुम लोग सुनते रहते हो। मगर, इसके अंदर जो अध्यात्म तत्व है, इसको तो हर एक संसार के विद्वान नहीं कह सकते। वो चीजें हम तुम्हें लखाने आये हैं। हम भागवत की कथा करने नहीं आये हैं, भागवत समझाने आये हैं तुम्हें। इसलिए जिज्ञासुओं ! भगवान के प्रेमियों इसको भैया निष्पक्ष हृदय से और विवेकिनी बुद्धि से इसे समझो और निष्पक्ष हृदय से इसे जानो। इस सिद्धांत में यहाँ पर किसी का खंडन-मंडन नहीं। किसी की आलोचना नहीं। किसी का विरोध नहीं। जी हाँ! जो सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किया जा रहा है। इसलिए सबके सब इसको ग्रहण करो और मानव जीवन का जो परम लक्ष्यहै-निजानन्द की प्राप्ति उसे प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी बनाओ। इस प्रकार से देवतागण स्तुति करके जाने लगे-
दिष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षाद् भगवान् भवाय नः ।
मा भूद् भयं भोजपतेर्मुमूर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः ।।
(10-2-41)
हे माता देवकी 'तवात्मजः यदूनां' तुम्हारा जो पुत्र है, वही आठवाँ है। ये कंस का काल होगा। कंस इसे नहीं मार सकेगा। तुम भय मत करो। जी हाँ। देवतागण कहकर चले गये भगवान के अवतार होने का समय आया। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और अर्द्ध रात्रि का समय ऐसे समय में -
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।।
(गीता अ. 4, श्लोक 7-8)
इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए देवकी के गर्भ से भगवान का अवतार कारावास के अंदर हो गया। कृष्णावतार ! जिस समय अवतार हुआ कारावास का अंधकार दूर हो गया। हथकड़ी-बेड़ी कट गई। पहरेदार सो गये और शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए भगवान ने दर्शन दिया। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य उपासना कांड की चारों मुक्तियाँ भगवान की चार भुजायें हैं। देवकी वसुदेव ने स्तुति किया तो भगवान ने कहा-यदि तुम को कंस से भय है तो मुझे अभी ले चलो गोकुल बाबा नन्द की पत्नी यशोदा जी के गर्भ से मेरी योग माया का जन्म हो चुका है। उसे ले आओ और मुझे वहाँ पहुँचाओ कह करके भगवान प्राकृत शिशु बन गये। पहरेदार सो गये। कारावास के कपाट खुल गये। महात्मा वसुदेव भगवान को लेकर चले। जब यमुना तट पर पहुँचते हैं तो कालिन्दी जो हैं यमुना उमड़ पड़ती है। भगवान का चरण स्पर्श करके रास्ता दे देती है। वसुदेव जी उस पार जाते हैं। नंद के भवन में जाकर भगवान को सुला देते हैं और योगमाया को लेकर वसुदेव जी कारावास में फिर आ जाते हैं। हथकड़ी, बेड़ी वैसे ही पड़ जाती है। अंधकार छा जाता है और योगमाया चिल्लाना शुरू करती है। पहरेदार जग जाते हैं और बताते हैं कंस को कि कोई पैदा तो हुआ, मगर ये पता नहीं कि पुत्र हुआ कि कन्या। कंस दौड़कर आता है। देखता क्या है कि कन्या। ओह ! आश्चर्य ! देवता भी झूठ बोलने लगे। अरे, आकाशवाणी हुई थी जो है सो आठवें गर्भ से पुत्र होगा। उठाया महारानी जी का चरण पकड़कर पटकना चाहा शिला पर उस समय योगमाया हाथ से निकलकर आकाश में चली गई।
भूमि रापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धि रेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।।
(गीता अ. 7 श्लोक 4)
ये अष्टधा प्रकृति महारानी की आठों भुजायें योगमाया की दिखाई दी। ललकार के कहती है कि- अरे मूर्ख कंस ! ये तू समझ ले कि आकाशवाणी असत्य नहीं भई, देवकी के गर्भ से पुत्र ही पैदा हुआ है, कन्या नहीं, कहकर अन्तर्द्धान हो जाती है। कंस डर जाता है। देवकी वसुदेव की हथकड़ी-बेड़ी काट देता है। दम्पत्ति अपने स्थान को आ जाते हैं। रात भर कंस चिंता मग्न रहता है। प्रातःकाल होते ही दैत्यों की जब सभा बुलायी जाती है। तब दैत्यों की सभा में अब जो प्रस्ताव पारित किया गया। अब वो प्रस्ताव कल सुबह 10 बजे सुनाया जायेगा।
हैं तो कालिन्दी जो हैं यमुना उमड़ पड़ती है। भगवान का चरण स्पर्श करके रास्ता दे देती है। वसुदेव जी उस पार जाते हैं। नंद के भवन में जाकर भगवान को सुला देते हैं और योगमाया को लेकर वसुदेव जी कारावास में फिर आ जाते हैं। हथकड़ी, बेड़ी वैसे ही पड़ जाती है। अंधकार छा जाता है और योगमाया चिल्लाना शुरू करती है। पहरेदार जग जाते हैं और बताते हैं कंस को कि कोई पैदा तो हुआ, मगर ये पता नहीं कि पुत्र हुआ कि कन्या। कंस दौड़कर आता है। देखता क्या है कि कन्या। ओह ! आश्चर्य ! देवता भी झूठ बोलने लगे। अरे, आकाशवाणी हुई थी जो है सो आठवें गर्भ से पुत्र होगा। उठाया महारानी जी का चरण पकड़कर पटकना चाहा शिला पर उस समय योगमाया हाथ से निकलकर आकाश में चली गई।
भूमि रापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धि रेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।।
(गीता अ. 7 श्लोक 4)
ये अष्टधा प्रकृति महारानी की आठों भुजायें योगमाया की दिखाई दी। ललकार के कहती है कि- अरे मूर्ख कंस ! ये तू समझ ले कि आकाशवाणी असत्य नहीं भई, देवकी के गर्भ से पुत्र ही पैदा हुआ है, कन्या नहीं, कहकर अन्तर्द्धान हो जाती है। कंस डर जाता है। देवकी वसुदेव की हथकड़ी-बेड़ी काट देता है। दम्पत्ति अपने स्थान को आ जाते हैं। रात भर कंस चिंता मग्न रहता है। प्रातःकाल होते ही दैत्यों की जब सभा बुलायी जाती है। तब दैत्यों की सभा में अब जो प्रस्ताव पारित किया गया। अब वो प्रस्ताव कल सुबह 10 बजे सुनाया जायेगा।
--------
पंचम दिवस
भगवान कृष्ण की बाललीला, ब्रह्मस्तुति, चीरहरण, उद्वव गोपी संवार, भ्रमर गीत
22-2-1969, प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
श्री मंगलाचरण - भगवान श्रीकृष्ण जन्म कथा के बाद से
यहाँ पर श्रीमद् भागवत के आधार पर आत्मतत्व का विवेचन हो रहा है। कल के प्रसंग में भगवान योगेश्वर श्री परम विश्वाधार के जन्म की कथा कही गाई थी। आज की कथा में उनकी बाललीला का प्रतिपादन किया जाएगा। जिस समय कंस को योगमाया द्वारा यह निश्चय हो गया कि वसुदेव की पुत्री नहीं वरन् पुत्र ही हुआ है, तो वह हताश हो वसुदेव और देवकी के कारागृह में छोड़ दिया। कंस को रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल दैत्यों की सभा बुलाई गई। दैत्यों ने इस महती सभा में अपना प्रस्ताव रखा कि महाराज हम लोगों ने रात्रि में ही यह निश्चय किया है कि इस राज्य में जहाँ भी बालक पैदा हुआ है, वह छोटा ही होगा-तो हम लोग दानवी माया करके राज्य की प्रजाओं के यहाँ जाकर अभी के उत्पन्न बालकों का वध करेंगे और इस तरह सुगमता से ही आपका शत्रु मारा जाएगा। बस, आपकी आज्ञा मात्र ही चाहते हैं। दैत्यराज कंस को यह प्रस्ताव पसंद आ गया और उसने आज्ञा दे दी।
अब यहाँ गोकुल में बाबा नंद के प्रांगण में पुत्र जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। गोप-गोपियों की अपार भीड़ हो गई। सुध-बुध भूलकर वे जन्म महोत्सव मनाये। इस उत्सव को देखने के लिए, देवलोक से सभी देवी, देवता, गोप-गोपियों का रूप ले सम्मिलित हुए। कंस द्वारा भेजे हुए पूतना, बकासूर, अघासुर, केशी भगवान का वध करने आये और बालकृष्ण के हाथ से उन सबका संहार हो गया और प्रभु के करकमलों द्वारा वध होने से सभी सारुप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। प्रभु बाल-लीला करते और गोप गोपियाँ एवं माता-पिता सभी को आनंदित करते। किसी दिन कोई गोपी अपनी एक सखी से कहती है-
श्रृणु सखि कौतुमेकं नंदिकेताङ्गणे मया दृष्टम् ।
गोधूलि धूसरिताङ्गो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ।।
अरि सखी ! आज बाबा नंद के प्रांगण में मैंने एक कौतुक देखा क्या देखा? गोधूलि धूसरित गौवों के चरणों की धूलि से वेष्टित वेदांत सिद्धांत को मैंने नाचते देखा। भगवान श्रीकृष्ण का नाम गोपियों ने वेदांत सिद्धांत रखा है। वेदांत सिद्धांत का क्या भाव है? वेद कहते हैं जानने को विद् ज्ञाने धातु से वेद शब्द बनता है। जिसको जानकर जानना कुछ बाकी न रहे-जानने का अंत हो जाये उसे कहते हैं वेदांत। वेदांत, भगवान आत्मा (विश्व की आत्मा) ही है। अब वेदांत का सिद्धांत क्या है? वासुदेवः सर्वमिति वासुदेव भगवान श्रीकृष्ण से भिन्न एक तृण भी नहीं, यही वेदांत का सिद्धांत है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सारे चराचर का अस्तित्व 'मैं' भगवान आत्मा हूँ और मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। यही वेदांत का सिद्धांत है। उस वेदांत सिद्धांत को आज मैंने बाबा नंद के प्रांगण में नाचते हुए देखा है। भगवान के लिए कितना सुंदर विशेषण गोपियों ने दिया है।
किसी दिन ब्रज के एक मार्ग पर कोई मस्ताना खड़ा है और मार्ग पर जाने वाले मुसाफिरों को पुकारकर कहता है-
मा यात पान्थाः पथिभीमस्थ्याः दिगम्बरः कोऽपि तमालनीलः ।
विन्यस्त हस्तोऽपि नितम्बबिम्बे धूतः समाकर्षति चित्तवित्तम् ।।
पान्थाः- हे पथिको ! तुम लोग इस समय इस मार्ग से न जाना, उधर मत जाओ ऐ मुसाफिरों ! वापस चले जाओ। इस गली में न जाना-यह गली बड़ी भयावह है। मुसाफिर पूछता है-भाई! आखिर इस गली में क्या भय है? उधर क्या है? क्यों रोकते हो? मस्ताना कहता है-देखो, इस गली में एक अवधूत बालक, बिल्कुल नंग-धड़ंग, कुटिल केशधारी श्याम रूप, बड़े अच्छे ढंग से टेढ़ी नजर किये खड़ा है- उसने अपने एक हाथ को तो ओंठ पर रखा है और दूसरा हाथ कमर पर। टेढ़ा खड़ा होकर मंद-मंद मुस्कुरा रहा है। सः किम् करोति-वह क्या करता है? हाँ सम्हलना। जो उसके सामने से निकल जाता है उसके चित्त रूपी धन को वह चुरा लेता है। बस, यही उसका काम है? भैया ! आत्मजिज्ञासुओं ! भगवान का नाम संतों ने रखा है चौराग्रगण्य। भक्तों ने प्रभु का नाम चोरों का सरदार (सरगना, अगुवा, मुखिया चोर) रखा है। उसे दुनियाँ की और चीजों से मतलब नहीं है, वह तो केवल चित्त ही चुराता है। भाई! जब वह अग्रणी चोर है तो कोई महत्व की चीज ही चुरायेगा। जान लो-वह तुम्हारी स्त्री का चोर नहीं, उसे धन नहीं चाहिए वह तुम्हारा धन न चुरायेगा, पुत्र का चोर नहीं है, इनकी वह चोरी नहीं करता। भगवान का नाम तो वित्तचोर है। देखो-समझना विषय-चौराग्रगण्य 'चित्त', इस चित्त से अब आधा 'त' निकाल लो, तो फिर क्या बचा? 'चित' तो जो चैतन्य घनभूत हैवह चोरी भी तो सिर्फ आधे 'त' की ही करता है। और यही तो चंचलता है। हैवा तनिकाल लो. तो चित शुद्ध चेतन तत्व भगवान का भगवान रह जाता है। तो बोरी का माल हुआ आधा 'त' और चोर हुए भगवान। बस, अब लगाओ हाजीरात हिन्द की दफा 379। हाँ भाई, चोर और चोरी के माल दोनों का पता लग गया।
यत्तु चंचलताहीनं तन्मनोऽमृतमुच्यते ।
तदेव च तपः शास्त्रसिद्धान्ते मोक्ष उच्यते ।।
(महोपनिषत् अ. 4.101)
जब तक जल में कंपन है तभी तक उसका नाम लहर है। कंपन न रहा तो लहर कहाँ, फिर तो जल ही जल है। जब तक कंपन है तभी तक लहर का अस्तित्व है। इसी तरह चित्त जब चंचलता से हीन होगा तो अमृत (आत्मा) ही होगा। शास्त्र में इसका ही नाम तप है और सिद्धांत में इसको मोक्ष कहते हैं। जी हाँ, तो समझना विषय-देखो, लहर देश में लहर है कि जल देश में? लहर देश में लहर है। जल देशमें जल ही जल है-इसी तरह चित्त देश में चित्त है न कि चित देश में। चित देश में तो चेतन आत्मा के अतिरिक्त चित्त नाम की कोई चीज ही नहीं है। (पू. श्री स्वामीजी ताली पीटकर शब्द विषय का अनुभव करा रहे हैं।) अनुभवकर्ता के देश में शब्द है कि शब्द अपने (शब्द) देश में है? शब्द देश में शब्द है, न कि आत्मदेश में। देखो, कोई भी विक्षेप हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पाँचों विषय हैं। इनके अनुभव का ही नाम विक्षेप है। गरज यह है कि चित्त जिससे विक्षिप्त हो उसका नाम विक्षेप है। बिल्कुल ठीक। अब यदि 'मैं' (आत्मा) देश में विक्षेप हो तो विक्षेप का अनुभव सदा होता रहे, परन्तु आत्मदेश में विक्षेप का अनुभव नहीं होता और विक्षेप देश में यदि विक्षेप है (विलक्षण भाव है, जरा समझना) तो विक्षेप नहीं। लकड़ी देश में यदि डंडा है तो डंडा नहीं, लकड़ी ही है और डंडा देश में डंडा है तो डंडा नहीं लकड़ी ही है। क्योंकि उसका अस्तित्व लकड़ी करके ही है। बिना लकड़ी के डंडा कहाँ, तो फिर डंडा भी न रहा। इसी तरह विक्षेप देश में विक्षेप है तो 'मैं' ही हूँ, विक्षेप नहीं और 'मैं' देश में विक्षेप है तो विक्षेप नहीं है 'मैं' ही हूँ। चित्त देश में चित्त है तो चित्त नहीं, चित ही है। यही चित्त की चोरी है। क्या जल के अनुभव में भी लहर है? जिस तरह जल देश में लहर नहीं इसी तरह चित देश में चित्त नहीं। चित देश में चित्त नाम की कोई चीज ही नहीं इसीलिए भगवान का नाम चौराग्रगण्य है तो माल का भी पता लग गया और चोर का भी। हाँ जी-भगवान जब कुछ बड़े हुए तो वही भिंड मुरैना (चंबल घाट) का गिरोह बनाये। भगवान ने गोप बालकों का एक गिरोह बनाया। बलराम जी, श्रीदामा, वृषपर्व आदि भगवान के सखा किसी दिन किसी गोपी के घर की तरफ से निकले तो पहिले गोपी के घर के सामने खूंटे से बंधे बछड़े खोल दिये। उन्हें छोड़ते ही बछड़े खेत की ओर भागे। अरे, हाँ भाई ! बंधन से खोलना तो भगवान का काम ही है। जब बछड़े खेतों की तरफ भागे तो अंदर से गोपी भागते हुए बछड़ों को पकड़ने दौड़ी, परन्तु जल्दी के कारण दरवाजे का संकल लगाना भूल गई। मौका अच्छा लगा। डाकुओं का गिरोह घर में घुस गया। खाली घर देख छीके के ऊपर जो मक्खन की हंडी थी उसे उतारकर यज्ञ पुरुष भगवान श्रीकृष्ण मक्खन निकालकर दबादब भोग लगाने लगे और सखाओं को भी खिलाने लगे। इसी समय जब घर की मालकिन गोपी वापस आई तो इन सबको मक्खन खाते देख वह पूछती है-यह क्या हो रहा है? तो भगवान और उनके सभी सखागण एक लाइन लगाकर खड़े हो गये। हाँ भाई, ट्रेन्ड जो थे। तो गोपी देखकर कहती है-
रे रे नंदशिशोः किमत्रभवने? मातुर्भयादागता,
एते के ? मम साक्षिणो, वदसखे किम गुह्यतम जंघयोः ?
चौर्यम् नात्र कृतम् मया च सुमुखि मार्जार संरक्षितम् ।
लग्न किं नवनीतमत्रवदने? लग्नं यशोदाकरात् ।।
अरे, अरे नंदनंदन ! बतला, बिना मेरी आज्ञा के, बिना पूछे तू मेरे सुने घर में क्यों आया है? कैसे आया है?
काम क्रोध मद मान न मोहा। लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा ।
जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया। तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया ।।
(अयो. रामा.)
इन विकारों से जो कि ऊपर चौपाई में दर्शाया गया है, जिसका हृदय रूपी मकान सूना है, रहित है, नंदनंदन भगवान श्रीकृष्ण उसी घर में आते हैं, उसके ही हृदय रूपी घर में प्रकाशित करते हैं। भगवान की अनुभूति तो सूने ही घर में होती है। देखने में आता है किसी मंदिर में कोई भगत आता है तो भगवान के दिव्य विग्रह के सामने इस मुद्रा में खड़ा हो जाता है। ( q , hat x स्वामी मुद्रा बनाकर बताते हैं।) धन्य हो गिरिधारी-आ जाओ, हे श्याम सुंदर। आ जाओ। तो फिर प्रभु कहाँ आ जाएं? तेरे हृदय में तो कूड़ा-कचरा भरा है। तूने हृदय में तो प्रपंच रूपी कूड़ा-कचरा भर रखा है, तो कहाँ आ जायें, तेरे सर पर?
लाज न लागत दास कहावत ।।
हरि निर्मल, मलग्रसित, असमंजस मोहि जनावत ।
जेहि सर काक कंक बक सूकर, क्यों मराल तहँ आवत ।।
(विनय 185)
लाज नहीं लगती तुम्हें दास कहाने में। अरे यार! जिस खड्डे में कीचड़ भरा है जो काक, बक, सूकर का स्थान है, जो शरीर मलमूत्र का भांड है तो क्या ऐसे गंदे स्थान में मराल-राजहंस पक्षी कहीं कभी आयेगा?
मिटैं जब दाग दिल के हरि का तब, हर जा तसव्वर हो ।
जो है बेदाग कपड़ा उस पे रंग, एकसार आता है ।।
अपने-आपको अधिकारी तो बनाओ, हृदय को साफ तो करो-विकार रूपी बगुले जहाँ हैं वहाँ तो भगवान नहीं आयेंगे।
हाँ, तो फिर गोपी कहती है कि मेरे सूने मकान में क्यों आये? भगवान कहते हैं-बड़ी मकान वाली बनी है, क्यों न आयें? मैया यशोदा दही बिलो रही थी, मैंने उससे हठ किया तो वह मुझे मारने दौड़ी। तेरे घर सूना पाकर इधर दौड़कर आ गया और अंधेरे में छुपा हूँ। अच्छा, तुम्हारी मैया तुम्हें मारने दौड़ी तो तुम छुपे हो परन्तु ये कौन हैं, ये फौज क्यों साथ में लाये हो? मम् साक्षिणः ये मेरे साक्षी हैं। तू नाहक झूठमूठ मुझ पर दोष न लगाये करके ये सब गवाह लाया हूँ। व्यर्थ ही हम पर दोषारोपण कर रही हो। तो बाबू जी ! यदि चोरी नहीं किया तो अपनी जांघों के बीच में क्या छिपा रखा है? श्रीकृष्ण भगवान मक्खन की छोटी मटकी फेंकना भूल गये थे और दोनों जांघों के बीच में मटकी दबाये खड़े थे। गोपी पूछती है-यह क्या है? क्या छिपाये हो? भगवान कहते हैं - अरी बाबरी ! देख-यहाँ पर बिल्ली तेरे मटकी का मक्खन खाने की ताक लगाई थी, उससे बचाने के लिए यहाँ छिपा रखा हूँ, मार्जार संरक्षितम्-उधर बिल्ली मक्खन खाने की ताक में बैठी, परन्तु उल्टा तू मुझ पर ही नाराज हो रही है। मैंने तो तेरे मक्खन को बिल्ली से बचाया है-नाराज न हो-बिल्ली से रक्षा कर रहा हूँ। गोपी कहती है- बाबूजी! चोरी नहीं की तो मुँह में क्या लगा है? लग्नं किं नवनीतमत्रवदने लग्नं यशोदाकरात्- भगवान कहते हैं कि यशोदा मैया दही बिलो रही थी और उसके हाथ में मक्खन लगा था। मैं वहीं था। तो उसने मक्खन लगे हाथ में मेरे मुँह में चपेड़ लगा दिया। वही मक्खन मेरे मुँह में लगा है, तेरे घर का नहीं है। गोपी आनंद विह्वल हो गई। इसी तरह भगवान व्रज में नाना प्रकार के व्रज वासियों को आनंद दे रहे हैं।
अब श्रीकृष्ण भगवान पाँच साल के हो गये तो उन्हें बछड़ों को चराने की अनुमति मिल गई। समवयस्क गोप बालकों को लेकर पास के जंगल (वृंदावन) में बछड़ों को चराने के लिए जाने लगे। किसी दिन अघासुर दैत्य बड़ा भारी अजगर का रूप धारण कर जंगल में जा बैठा। श्रीकृष्ण पर घात लगाकर जंगल में मुँह बाये (मुँह खोलकर) बैठ गया। श्रीकृष्ण उसका भी उद्धार किये। उसे जब मार दिये तो सारे संसार भर में हलचल मच गई कि बाबानंद के पुत्र श्रीकृष्ण ने बड़े भारी बलवान अघासुर दैत्य का वध कर दिया। यह कोलाहल ब्रह्मलोक तक पहुँचा। माया ठगनी बुढ़उ को भी न छोड़ी। माया बुढ़उके सिर जा बैठी। ब्रह्माजी को मोह हो गया कि वृंदावन में नंद का बालक पाँच साल का श्रीकृष्ण इतने प्रतापी अघासुर दैत्य का वध कैसे किया-चलो, वहाँ जाकर उसकी परीक्षा लें, देखें तो सही कि वह कितना बलशाली है?
देखो, यह वही ब्रह्माजी हैं, जो भगवान श्रीकृष्ण के अवतार के समय गर्भस्तुति करने आये थे। माया किसी को नहीं छोड़ती, सबको रगड़ मारती है।
माया महाठगिनि हम जानी ।
केशव के कमला होय बैठी, भव के भवन भवानी ।
पंडा के घर मूरति होय बैठी, तीरथ में भई पानी ।।
(री माया…)
ठगनि क्या नैना चमकावै ।
कद्दू काटि मृदंग बनाई, नींबू काटि मंजीरा ।।
साग तुरैया मंगल गावैं, नाचै बालम खीरा ।।
(री ठगनि क्या..)
भैंस पद्मिनी चूहा आशिक, मेंढ़क ताल लगावै ।
छप्पर चढ़िकै गदहा नाचै, ऊँट विष्णु पद गावै ।।
(री ठगनी क्या...)
मतलब? ब्रह्मा जी परीक्षा लेने वृन्दावन में आये। दोपहर का समय था। श्रीकृष्ण भगवान बाल गोपाल के साथ दही-भात का भोजन कर रहे थे और कुछ दूर पर बछड़े हरी-हरी घास आनंद से चर रहे थे। भगवान श्रीकृष्ण ने देखा कि ब्रह्माजी बड़ी दूर ब्रह्मलोक से आये हैं तो उन्होंने गोप बालकों को आदेश दिया कि देखो, बछड़े जो हैं वे चरते-चरते बड़ी दूर निकल गये हैं, अतः उन्हें हाँककर ले आओ। अब ब्रह्माजी को एकांत मिला तो उन्होंने बछड़ों एवं गोप बालकों को हरण कर लिया और ले जाकर ब्राह्मी गुफा में सबको सुला दिया। फिर लग गये अपने काम (सृष्टि करने) में। इधर भगवान श्रीकृष्ण बछड़ों एवं गोप बालकों को न देखकर समझ गये कि ब्रह्माजी ने उनका हरण कर लिया है। अब क्या होता है-
यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराङ्घयादिकं ।
यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावद्विभूषाम्बरम् ।
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं ।
सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ ।।
(श्रीमद् भागवत 10 - 13 - 19 )
जितने बछड़े थे, जैसा उनका रूप रंग था, जैसे उनके खुर, सींग इत्यादि थे। जैसे उनके चराने वाले गोप, बालक जैसा उनका रूप, रंग, आकार, अवस्था, वस्त्र, आभूषण, छड़ी, बांसुरी, सींग का बाजा, खेलकूद, स्वभाव सब भगवान श्रीकृष्ण वैसे और उतने ही हो गये। हो गये, बने नहीं। भैया ! बनना और होना में बड़ा अंतर है। जो वस्तु पहले से हो उसे होना कहते हैं। और जो पहले से न हो उसे बनना कहते हैं। जैसे कि कन्या जो है वह माँ के गर्भ से ही स्त्री होकर आती है, बनती नहीं। चटकना, मटकना ऐसे देखो, वैसे न देखो क्या कोई इन्हें सिखाता है? क्या कहीं इनका ट्रेनिंग स्कूल है? और हिजड़े स्त्री बनते हैं, होते नहीं। हैं तो वे पुरुष ही, परन्तु स्त्री बनते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्रीकृष्ण हो गये, क्योंकि पहले से ही सब कुछ वही थे। रोज बछड़ों को चराने ले जाते और संध्या होते-होते वापस लौट आते, परन्तु इस रहस्य का पता गौवों एवं गोप बालकों की माताओं को भी नहीं लगा।
जिज्ञासुओं ! इस कथा से कौन-सी शिक्षा लेनी चाहिये? स्थूल, सूक्ष्म, कारण सभी भगवान हैं। भगवान आत्मा के बिना एक क्षण भी नहीं। वासुदेवः सर्वमिति गोपियाँ सभी अपने-अपने बालकों को वापस आने पर प्यार करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि वे उन्हीं के बालक हों-प्रेम वही, लीलाएं वही, गौएं अपने बछड़ों को पाकर वैसे ही प्रेममय थीं जैसे उनके ही बछड़े हों। कोई संदेह, झिझक नहीं, नाम का नहीं-सभी कार्य पूर्ववत् चलता रहा। जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वर्ष बीत गया-इतने दिन बाद ब्रह्माजी को ख्याल आया तो सोच में पड़े और तुरंत संकल्प हुआ कि चलकर वृंदावन में देखें तो सही। हंसवाहन ब्रह्माजी हंस पर आरुढ़ हो वृंदावन आते हैं। उनके अचरज का कोई पारावार नहीं रहा-उन्हें सारा वृंदावन कृष्णमय दिखाई दिया। क्या देखते हैं कि एक-एक श्रीकृष्ण भगवान की सेवा में दस-दस ब्रह्मा लगे हैं। जो ब्रह्मा ब्रह्म लोक से आये थे, वे तो चतुरानन थे। सब यहाँ पंचानन, षडानन, दशानन, शतानन, सहस्त्रानन, अनन्तानन ब्रह्मा उन्हें दिखाई देने लगा। सभी भगवान श्रीकृष्ण की सेवा में रत थे। अनेकानेक ब्रह्माण्ड के ब्रह्मा वहाँ एकत्र थे। देखकर ब्रह्माजी के होश उड़ गये, चकरा गये, एक ब्रह्मा हो तो, वहाँ तो ब्रह्माओं की गिनती नहीं, इतने ब्रह्मा। ब्रह्माजी अभी तक अपने को ही एकमात्र ब्रह्मा जानते थे, इसलिए ब्रह्माजी काठ की पुतली के समान स्तंभित रह गये। मैं ब्रह्मा सत्य हूँ या ये सब ब्रह्मा सत्य है? देखो-ब्रह्माजी को मोह क्यों हुआ? अरे भाई ! समझना विषय-मैं ब्रह्मा हूँ, इस भाव में ब्रह्माजी को मोह हुआ। है चीज वही, उसे कुछ मान लेना ही मोह है। माया कहीं बाहर से नहीं आती।
माङ्-माने, धातु से माया बनता है। जो माना जाय, उसका नाम माया और जिसको माना जाय वह मायापति। पा-रक्षणे धातु से पति शब्द बनता है। जिसके बिना जो न रहै, वही उसका पति है। जो रक्षा करै उसका नाम पति है। इस डंडे से लकड़ी निकाल लो तो डंडा नहीं रहेगा इसलिए इस डंडे का पति लकड़ी है। डंडे का पति लकड़ी, कपड़े का पति सूत, आभूषण का पति सोना, घड़े का पति मिट्टी। जो जिसकी रक्षा करे वही उसका पति, जो जिसका कारण हो, जो आधार हो, जो जिसमें व्यापक हो, जो जिसका अस्तित्व हो, वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। यह नियम है। जो माना जाय उसका नाम माया। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सारे चराचर की जो मान्यता है, इस मान्यता का आधार 'मैं' आत्मा हूँ। ये सब मुझ पर ही तो आधारित है। सारा प्रपंच मायापति पर आधारित है। उसको माया का पति कहो या माया का आधार ।
शिव विरंचि कहुँ मोहइ, को है बपुरा आन ।
अस जिय जानि भजहिं मुनि, मायापति भगवान ।।
अस जिय जानि के मानि। मजा आ गया। माया को माना गया और किसको जान? 'मैं' आत्मा (मायापति भगवान) को। तो ब्रह्मा काठ की पुतली की नाई देख रहे हैं?
थोड़ी ही देर में वृन्दावन भूतपूर्व दिखाई देने लगा और भगवान श्रीकृष्ण और एक ब्रह्मा रह गये जो कि ब्रह्मलोक से आये थे। तब उन्हें होश आया और हंस पर से उतरकर किरीट मुकुट पृथ्वी पर रखकर दंड प्रमाण कर स्तुति करते हैं।
(यह ब्रह्मस्तुति 40 श्लोकों में है। श्रीमद् भागवत दशमस्कन्ध चौदहवाँ अध्याय)- ब्रह्मोवाचः
नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय ।
वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ।।
(श्रीमद् भागवत 10-14-1)
इडितुम् योग्यः तत् सम्बुद्धौ हे इड्य, हे स्तुत्य, ते तौ तुभ्यम् अहम् नौमि । स्तुति करने योग्य जो तुम इसलिए तुम्हारा मैं नमस्कार करता हूँ। तुम कैसे हो? अधवपुषे-अभ्रवत् वपुः शरीरं यस्य सः अभ्रवपुषे। अभ्र माने आकाश के सामान निर्मल शरीर है जिसका, उसे कहते हैं अभ्रवपु या अभ्रवत् मेघवत् वपुः सः अभ्रवपुः तस्मै अभ्रवपुषे। अभ्र माने मेघ के समान नीलवर्ण का शरीर है जिनका इसलिए अभ्रवपु अथवा अभ्र एवं वपुः अभ्रवपुः तस्मै अभ्रवपुषे- आकाश ही है शरीर जिसका।
य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः शरीरं ।
य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याभ्यमृतः ।।
(3-7-12 वृहदा)
जो आकाश के भीतर बाहर स्थित है, जिसको आकाश नहीं जानता और जो आकाश को जानता है, आकाश ही जिसका शरीर है-वही आत्मा अन्तर्यामी अमृत स्वरूप है। और फिर आप कैसे हैं। तडिदम्बराय अर्थात् भगवान जो पीताम्बर धारण किये हैं उसमें विद्युत के समान प्रतिभा (छटा) है। गुञ्जावतंस परिपिच्छल-सन्मुखाय-भगवान् ! आप कानों में घुंघची (जंगली गोमची के बीज) के समूहों का कुंडल धारण किये हैं, सिर पर मयूर के पंख का मुकुट है और आप मंद-मंद मुस्करा रहे हैं। वन्यस्रजे जंगली पुष्पों की वनमाला धारण किये हुए हैं, एक हाथ में दही-भात का कौर है, दूसरे हाथ में छड़ी, मृगा के सींग का बाजा जो कि ग्वालिये बजाते हैं, रखे हुए हैं, बगल में बंशी दबाये हुए हैं। फिर आप कैसे हैं? लक्ष्मश्रिये मृदुपदे-सुंदर कोमल-कोमल आपके चरणारविन्द हैं जो महारानी लक्ष्मी जी द्वारा सेवित हैं और आप कैसे हैं। पशुपाङ्गजाय-पशून् पातीति पशुपोनंदः तस्य अंगः पशुपाङ्गः तस्मात् जातः पशुपाङ्गजः तस्मै पशुपाङ्गजाय-पशु यानी गौवों के प यानी पालक बाबा नंद उनके अंग से तुम हुए हो इसलिए पशुपाङ्गजः। अथवा पशुप बाबा नंद उनके अंग यानी मित्र वसुदेवजी उनसे तुम पैदा हुए हो इसलिए तुम्हारा नाम पशुपाङ्गज है, क्योंकि अंगश्च्य दैत्यः सखा इत्यमरः। अंग कहते हैं दैत्य को और अंग कहते हैं मित्र को। पशवः संसारिणो जीवाः तेषाम् पपालकाः वयं ब्रह्मेन्द्र रुद्रादयः ते सर्वे भगवदङ्गात् जातः पशुपाङ्गजाय तस्मै पशुपाङ्गजाय। पशु रूप संसारी जीव उनके प माने पालक हम लोग स्रष्टा भर्ता, हर्ता, ब्रह्मादिक सभी आपके अंग से पैदा हुए हैं इसलिए आपका नाम पशुपाङ्गजः है। पशवो वत्साः प पालकाः गोपबालकाश्च ते सर्वे भगवङ्गात् जातः पशुपाङ्गजः तस्मै पशुपाङ्गजाय। पशु यानी बछड़े, उनके पालक गोप बालक, ये सभी आपसे हुए हैं। अर्थात् बछड़े एवं बालक सब कुछ आप ही हो गए हो इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ।
नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय ।
वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ।।
एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः ।
नित्योऽक्षरोऽजस्त्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः ।।
(10-14-23)
भगवन् तुम एक हो और एक होते हुए आत्मा हो, इस श्लोक में एक के आगे आत्मा शब्द आया है, क्योंकि आत्मा ही एक है, बाकी सब अनेक है। फिर कहते हैं-पुरुष क्यों? यहाँ पर पुरुष का अर्थ स्त्री-पुरुष लिंगवाचक शब्द नहीं है, ऐसा शब्द न समझना। पु-पुर्याम् शेते यः सः पुरुषः। साढ़े तीन हाथ की पुरी में जो विश्राम करता है उसे कहते हैं पुरुष पुराणः पुरी का तो नाश हो जाता है, परन्तु उसमें जो व्यापक तत्व है आत्मा उसका नाश नहीं होता इसलिए पुराण है। भगवन् आप अजन्मा हो अर्थात् आपके जन्म का पता ही नहीं है। अब प्रश्न होता है कि पुराना तो अज्ञान भी है-अज्ञान कब पैदा हुआ, इसकी भी जन्मकुंडली जन्म संवत नहीं है। तो कहते हैं सत्य अर्थात् आप अनादि और अनन्त हैं, परन्तु अज्ञान अनादि और सान्त है। फिर आप कैसे हो? स्वयं ज्योतिः अर्थात् आप स्वयं प्रकाश हो तो कहते हैं कि स्वयं प्रकाश तो सूर्य भी है, तो आप सूर्य हो? नहीं! अनन्तः अर्थात् आप अनन्त हो, परन्तु सूर्य का प्रकाश तो आदि अन्त वाला होता है, सूर्य का तो उदय-अस्त होता है। आप आद्य हो। नित्यः नित्य हो? अब प्रश्न होता है कि नैयायिक आकाश को नित्य मानता है, तो क्या आप आकाश हो? तो कहते हैं-नहीं, अक्षरः अर्थात् अविनाशी हो। अजस्त्र हो। सुख स्वरूप हो। निरञ्जन माने निर्विकार हो, पूर्ण हो, अद्वय माने एक हो, मुक्त हो, उपाधिरहित और अमृत हो।
एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते ।
गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सुचक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम् ।।
(10-14-24)
एवं विधं त्वां इस प्रकार जो तुम हो, तो तुम्हारा दर्शन कैसे हो? कहाँ पर हो? किस करके हो? और किसको हो? गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा-यहाँ ब्रह्मा जी ने गुरु की उपमा सूर्य से दी, क्योंकि जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के वचन रूपी किरणों से अनादिकाल से अज्ञानान्धकार का नाश हो जाता है। सूर्य रूपी गुरु और उपनिषत्सुचक्षुषा-यानी उपनिषद् रूपी आँख से उपनिषद् शब्द व्याकरण के षट्लृविशरणगत्यवसादनेषु धातु से बनता है। उप और नि उपसर्ग हैं। जो परमात्मा के समीप पहुँचा दे उसको कहते हैं उपनिषद। संसार विनाशयति संसारस्य मूलकारणं अविद्यां शिथिलयति, ब्रह्म च गमयति इत्युपनिषद्। जो संसार का नाश करे, संसार के मूल कारण अविद्या को शिथिल करे और सनातन ब्रह्म आत्मा को प्राप्त करा दे उसे उपनिषद कहते हैं। सूर्य रूपी गुरु और वेदान्त रूपी नेत्र के द्वारा अपनी आत्मा करके आत्मा में आत्मा को जो तुमको परमात्मा देखते हैं, यानी 'मैं' करके 'मैं' में 'मैं 'को जो तुमको परमात्मा देखते हैं, जानते हैं-ये तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्-वे इस असत्य संसार सागर से तर जैसे जाते हैं। बुढ़उ (ब्रह्मा) का वचन बड़ा विलक्षण है-तर जैसे जाते हैं, तरते नहीं। क्योंकि यदि संसार हो तब तो तरा जाय और जब संसार है ही नहीं, संसार है इस विकल्प का ही नाम संसार है तो फिर तरेगा किसको ? इसलिए तर जैसे जाते हैं।
रजत सीप महँ भास जिमि यथा भानु कर वारि ।
जदपि मृषा तिहुँ काल सोई भ्रम न सकइ कोउ टारि ।।
(बा.का.)
जब संसार है ही नहीं तो इससे तरेंगे क्या? संसार को यहाँ पर मृषा कहा गया है और आगे की चौपाई-
एहि विधि जग हरि आश्रित रहई। यदपि असत्य देत दुःख अहई ।।
में असत्य (अनृत) कहते हैं। तो संसार मिथ्या भी है और असत्य भी। समझो-असत्य और मिथ्या दोनों के अर्थ अलग-अलग होते हैं। जो उत्पन्न होकर नाश हो जाय उसे मिथ्या कहते हैं और जो तीनों काल में है ही नहीं, अविद्यमान हो, वन्ध्यापुत्रवत् है, उसे असत्य कहते हैं। यहाँ संसार को असत्य कहा गया है और भागवत के श्लोक में अनूत कहा गया है अर्थात् संसार है ही नहीं। अरे भाई। रस्सी में जो सर्प दिखता है वह मिथ्या भी है और असत्य भी है। इसी तरह शरीर मिथ्या भी है और असत्य भी। उत्पन्न होकर नाश हो जाता है इसलिये मिथ्या है और शरीर है ही नहीं इसलिए असत्य है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब आगे इसकी अपील नहीं हो सकती। शरीर देश में शरीर मिथ्या है और आत्मदेश में शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं है इसलिए शरीर असत्य है। संसार, संसार देश में मिथ्या है और आत्मदेश में है ही नहीं इसलिए संसार असत्य है। यह अटल सिद्धांत है। टस से मस नहीं होना है। अकाट्य सिद्धांत है।
एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते ।
गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सुचक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम् ।।
सूर्य रूपी गुरु से उपनिषद रूपी नेत्र द्वारा अपने 'मैं' को अपने 'मैं' में जो तुमको परमात्मा देखते हैं, जानते हैं, वे इस असत्य संसार सागर से तर जैसे जाते हैं। अच्छा भैया ! मैं आत्मा को परमात्मा देखना क्या है? मैं आत्मा को सिर्फ 'मैं' ही कहना या 'मैं' के साथ मैं आत्मा जोड़ना एक ही है। अनादिकाल से अपने आपको 'मैं' का अर्थ साढ़े तीन हाथ का शरीर लगाये हो इसलिए गलती से 'मैं' का मतलब शरीर न मान लो करके मैं के साथ आत्मा कहा जाता है। नहीं तो 'मैं' का अर्थ आत्मा ही होता है।
समझो विषय-'मैं' आत्मा को परमात्मा कैसे देखें? देखो-मैं परमात्मा हूँ, ऐसा कहना मान्यता है भला और जहाँ तक मान्तया है वहाँ तक माया ही है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं व्यापक हूँ ऐसी मान्यता भी माया के अंदर है। भगवान देश में जानना और माया देश में मानना। जी हाँ-भगवान देश में 'जानना' ऐसा शब्द है और माया देश में मानना ऐसा शब्द है। तो फिर मैं भगवान हूँ, ऐसा कहना भी मानना हो है। यह जानना नहीं है। यह देखना नहीं है, अनुभव करना नहीं है। तो फिर आत्मा को परमात्मा कैसे देखते हैं? जानना क्या है? क्या भगवान भी अपने आपको मैं भगवान हूँ, ऐसा कहता है? यदि ऐसा भगवान कहें कि मैं भगवान हैं, तो उसकी महिमा कहाँ रहे। मैं भगवान हूँ, ऐसा भगवान कहें, तो मैं भी आपने आपको मैं भगवान हूँ, कहूँ। परन्तु जब भगवान ही मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं कहता तो 'मैं' क्यों कहूँ कि मैं भगवान हूँ। बस, यही भगवान को देखना है। अरे हाँ! जीव कैसे भगवान होगा? अभी तक अपने को जीव माना था, अब जीव से कुछ बड़ा अपने को भगवान मानता है। अतः जब तक अपने आपको भगवान भी मानता है, तब तक अपने-आपको जानता नहीं, यह भी मानना ही है। माया ही है।
बड़ी विचित्र बात है। यह सूक्ष्म तत्व है। अपने मैं आत्मा को भगवान नहीं जानेगा तो भगवान में अपने 'मैं' को देखेगा। भगवान में अपने 'मैं' को देखनाक्या है? 'मैं' को 'मैं' ही जानना, यही भगवान में अपने 'मैं' को देखना है। भगवान, परमात्मा, ब्रह्म इन नामों को किसने रखा है? भक्तों ने नामकरणकिया है। पैदा भी तो वे ही करते हैं। अरे ! भक्त न हो तो भगवान को पैदा कौन करे? शिव-तो भैया ! भक्तों ने ही नाम रखा है। परमात्मा, परमतत्व भगवान। जी हाँ उसको क्या मुसीबत पड़ी है मुनादी करने की कि मैं भगवान हूँ। मैं भगवान हूँ, तब कहे जब उसको दूसरा दिखाई दे। ढिंढोरा पीटे तब जब उसे अपनी आँख में दूसरा दिखाई दे। जहाँ अंधकार का अत्यन्ताभाव हो उसे सूर्य कहते हैं। सूर्य को अंधकार से कहना न पड़ेगा कि मैं सूर्य हूँ जबकि सूर्य के प्रगट होने पर अंधकार का अपने आप अत्यन्ताभाव हो जाता है। फिर सूर्य किस अंधकार से कहेगा कि मैं सूर्य हूँ, जबकि वहाँ अंधकार का नामोनिशान ही नहीं है। इसी तरह जहाँ प्रपंच का अत्यन्ताभाव हो उसे भगवान कहते हैं। भगवान में विकल्पभाव नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो अंधकार का प्रतिद्वन्द्वी है। अतः सूर्य के प्रकाश से अंधकार नहीं देखा जा सकता। तो फिर वह कौन-सा प्रकाश है, जिससे कि अंधकार और प्रकाश दोनों का ज्ञान होता है। यह मुझ भगवान आत्मा का प्रकाश है। यदि भगवान के स्मरण में तुम्हें मन दिखाई देता है तो तुम मन का ही स्मरण कर रहे हो, भगवान का स्मरण नहीं। प्रकाश के ध्यान में अंधकार कहाँ-
महाराज अब ध्यान लगाये बैठे हैं-परन्तु भगवान के ध्यान करने में मन पता नहीं कित्थे जाता है। भगवान के ध्यान से और मन से क्या ताल्लुक? भगवान अपनी जगह में और मन अपनी जगह में। इस सिद्धांत को समझने में बड़े-बड़े वेदान्ती चक्कर में पड़ जाते हैं। मन का चक्कर नहीं जाता। क्या आत्मदेश में भी मन है। वहाँ पर तो मन का अत्यन्ताभाव है। प्रपंच, शरीर, मन, सृष्टि ये सब माया देश की बात है, भगवान देश में ये कहाँ? स्वामी जी ! तो फिर क्या भगवान का भजन नहीं करना चाहिए और भगवान का भजन क्या है? (स्वामी जी कहते हैं) हाँ भाई। यह फिर बतायेंगे, यह बात फिर कहेंगे। जी हाँ- भगवान का भजन करना यही है कि बस, कुछ न करो। हाँ भाई ! हमारी बात मानों तो औरों के भजन में तो करना, धरना है, परन्तु भगवान के भजन में कुछ करना धरना नहीं है। क्योंकि, भजन करोगे तब न तरोगे और भजन न करोगे तब न तरोगे, इसलिए भजन करना चाहिए। भैया ! जिसकी शादी होती है, गीत तो उसी का गाया जाता है। ब्रह्म स्तुति आध्यात्मिक विषय है। यदि संसार सत्य है तो उसको तरा नहीं जा सकता और संसार असत्य है तो है ही नहीं, तरोगे किसको? अगर आवागमन सत्य है तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी और असत्य है तो आवागमन है ही नहीं, तो फिर निवृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। सब तरह से मुसीबत है।
एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते ।
गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सुचक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम् ।।
(10-14-25)
अब प्रश्न होता है कि जब संसार है ही नहीं तो प्रपंच आता कहाँ से है? आत्मानमेवात्मतयाविजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम् । ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्जवामहेर्भोगभवाभवौ यथा ।।
भैया ! सुनने में कि 'कुछ न करना' यह बड़ा सरल लगता है, परन्तु यह इतना कठिन साधन है कि लाखों में कोई एक इसको समझता है। संसार सागर से तरने के लिए कुछ न करना, सुनने में यह बड़ा आसान दिखता है। स्वामी जी! तब क्या कुछ न करना चाहिए? अरे ! अनादिकाल से टांगे का जुता हुआ घोड़ा क्या कुछ न करेगा? जुता रहा तो फिर अवश्य कुछ न कुछ करेगा ही। और भाई! अभी तक कुछ करके क्या कमाये? नाना प्रकार के साधन किये परन्तु क्या मिला? स्वर्ग-इसका अनुभव तो किये ही हो। अब अभी जो पुड़िया दी जा रही है उसका भी सेवन करो, पुड़िया पेट में गई नहीं कि मर्ज और मरीज दोनों खतम हो जाते हैं। जब तक मर्ज है तब तक मरीज भी है, परन्तु इस पुड़िया से मर्ज मरीज दोनों खत्म हो जाते हैं। बड़ा कठिन साधन है लाखों करोड़ों में कोई-कोई इसे पकड़ता है। दंड, कमंडल धारण किये हुए सिद्ध आपको बहुत मिलेंगे, परन्तु अनारंभ व्रती होना, कुछ न करो, मत करो, क्या यह मामूली चीज है?
आत्मानमेवात्मतयाविजान्तां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम् ।
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवौ यथा ।।
यह प्रपंच आया कहाँ से? अपने स्वरूप आत्मा के अज्ञान से, निखिलं प्रपञ्चितम् सारा संसार पैदा हो जाता है। अपने स्वरूप आत्मा से प्रपंच की उत्पति हो जाती है और ज्ञान होने पर, जहाँ से पैदा हुआ था वहीं जाकर लीन हो जाता है। अब इस पर रज्जु और सर्प का दृष्टान्त देते हैं।
अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता ।
सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्मा विकल्पितः ।।
(माण्डू गौ. का. वैतभ्य.प्र.-17)
अंधकार में रस्सी पड़ी है। रज्जु पर जब सर्प का विकल्प करोगे, तो सर्प ही सर्प है। हालांकि सर्प है नहीं, न अंधकार में, न प्रकाश में। वस्तुतः वह रस्सी ही है। परन्तु, रज्जु के अज्ञान से जिस तरह रज्जु में सर्प का विकल्प होता है, इसी प्रकार अस्तित्व भगवान आत्मा के अज्ञान से मैं आत्मा पर जगत का विकल्प होता है।
'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः' अर्थात् सुनाई तो पड़े, परन्तु वस्तु का अभाव हो, ढूँढने पर वस्तु न मिले उसे कहते हैं विकल्प। रज्जु का निश्चय हो जाने पर अंधकार से उत्पन्न सर्प के विकल्प का अत्यन्ताभाव हो जाता है और यही निश्चय होता है कि अरे! यह तो रज्जु ही है। ऐसा नहीं कि पहिले सर्प था और प्रकाश होने पर रज्जु हो गया। रज्जु का सर्प मिथ्या भी है और असत्य भी। सर्प देश में सर्प मिथ्या है और रज्जु देश में सर्प असत्य है, है ही नहीं। इसी तरह अपने मैं आत्मा के अज्ञान से संसार प्रपंच पैदा हो जाता है और स्वरूप ज्ञान (आत्म का बोध) हो जाने पर प्रपंच (संसार) का जो विकल्प है उसका अत्यन्ताभाव हो जाता है। फिर यही अनुभव होता है कि 'मैं' आत्मा ही हूँ- मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। अरे भाई ! विकल्प का कोई आधार भी तो होना चाहिये। मुझ आत्मा के अतिरिक्त इसका आधार कौन होगा, इसलिए इस संसार (जगत, प्रपंच) विकल्प का आधार मैं आत्मा ही हूँ। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सारे विश्व का आधार कौन? मैं आत्मा हूँ। रामायण में भी कहा गया है कि-
झूठेहु सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ।।
जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन भ्रम जाई ।।
निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते ।
रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्म विनिश्चयः ।।
(18 गौ.का. वैतथ्य प्र.मा.)
जी हाँ अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि रज्जु में जो सर्प का भ्रम है यह असत्य है, हम समझ गये, ठीक है। परन्तु जिसने अपने जीवन में सर्प कभी नहीं देखा है तो ऐसे व्यक्ति को रज्जु में सर्प का भ्रम कैसे होगा? ऐसा प्रश्न संसार का अस्तित्व स्वीकार करने वाले पूर्व पक्षियों का है। भौतिकवादियों का यह प्रश्न है। जिसने जिस चीज को अपने जीवन में कभी नहीं देखा उसे उसका भ्रम नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिसने अपने जीवन में सर्प नहीं देखा तो उसको रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा है। संसार भास रहा है। तो जनाब ! जो कभी देखा हो, उसी का भ्रम हो ऐसा नहीं, सुने हुए का भी भ्रम होता है। संसार का प्रवेश दो ही इन्द्रियों द्वारा होता है, आँख और कान। नाम, रूप ही तो संसार है। अर्थात् भ्रम देख करके या सुन करके ही हो सकता है। सर्प देखा था इसलिए न, सर्प का भ्रम हुआ अच्छा, भला बताओ, इतने बैठे हो, किसी ने कभी प्रेत देखा है या सिर्फ बाप-दादों से सुनते चले आ रहे हो? उसके बाप ने उसको बतलाया, उसके बाप ने बाप को बतलाया। इस तरह परम्परा से सबके हृदय में प्रेत बैठा हुआ है-देखा किसी ने भी नहीं है। ओ पाण्डेय जी ! कल आप रात्रि में कहाँ गये थे? भैया ! मैं स्वामीजी का भागवत सुनने झंडापुर चला गया था और किसी कारणवश वहाँ से लौटने में मुझे देर हो गई। क्या, ज्यादा रात्रि में वापस आये? हाँ अरे ! 11-12 बजे के लगभग रहा होगा। क्या आप अकेले रहे हो? भैया तुम उसी सड़क से आये होगे जहाँ बड़ा भारी पीपल का पेड़ है। हाँ भाई-अकेला ही रहा और वही तो रास्ता है। उधर से ही आया हूँ। न जाने तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई जो कि उधर से अकेले आये हो? बस, इतना ही काफी है-अब ज्यादा ब्यौरा बतलाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब पाण्डेयजी की क्या हिम्मत है कि उस रास्ते में रात्रि में निकलें। पाण्डेय महाराज के तो रोंगटे खड़े हो गये। भैया हम तो मरते-मरते बचे थे। एक समय हम भी बिहार का बाजार गये थे। हमें भी देर हो गई थी, दादा, मरते-मरते बचे-पीपल के पेड़ के पास हर-हर-हर बाप रे बाप-हम तो अब पाण्डेयजी की क्या हिम्मत है जो कि उधर से निकलें। लो, पिशाच की भ्रांति हो गई। हालांकि उसने जिंदगी में कभी पिशाच देखा नहीं है। परन्तु सुनने में ही भ्रान्ति दृढ़तापूर्वक हृदय में बैठ गई। यह श्रवण भ्रान्ति है। बाप-दादे से सुनते आये हैं कि पिशाच है, देखा नहीं तो क्या हुआ? यह कोई जरूरी नहीं है कि भ्रान्ति देखी हुई चीज की ही होती है। अनादिकाल से संसार का विकल्प हो रहा है कि यह संसार है और संसार की सृष्टि, पालन, संहार ऐसा होता है। इस प्रकार सुनते चले आये हैं। अनादिकाल से संसार विकल्प हृदय में बैठा हुआ है, दूँठ में पिशाच का दिखना। किसी ने कहीं रास्ता चलते दूर में अंधेरे में एक बबूल का दूँठ देख लिया तो उसके मन में पिशाच का भ्रम हो गया। अब लगा ब्रह्म गायत्री का पाठ करने पिशाच को भगाने के लिए ब्रह्म गायत्री का पाठ कर रहे हैं। परन्तु सब पूजा-पाठ फेल हो गये। ब्रह्म गायत्री पिशाच को भगाने के लिए है न कि दूँठ को भगाने के लिए। बबूल के दूँठ को भगाने का काम ब्रह्म गायत्री से तो न होगा। जिस अंधकार के कारण दूँठ में पिशाच का भ्रम हो रहा है, जब तक वह दूर न होगा, तब तक पिशाच न भागेगा। जब प्रकाश में ठूंठ को देख लेगा, जान लेगा कि यह दूँठ है तभी उसकी भ्रान्ति मिटेगी, अन्यता नहीं। इसी प्रकार 'मैं' आत्मा में, अनादिकाल से अज्ञानान्धकार के कारण संसार दिख रहा है, उसका नाश प्रकाश (स्वरूप ज्ञान) से ही होगा अर्थात् जब अपने में आत्मा को जान लोगे तो संसार का भ्रम दूर हो जायेगा। देखो-यदि संसार प्रतीत हो तो संसार को सत्य मानना पड़ेगा। फिर दो सत्य हो जाएगा-एक संसार और दूसरा भगवान। परन्तु ऐसा नहीं, सत्य एक ही होता है इसलिए संसार है ही नहीं। तो फिर बंध कहाँऔर जब बंध नहीं तो मोक्ष कहाँ-
अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात् ।
अजस्त्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ।।
(10 - 14 - 26)
भव बंध मोक्षौ अज्ञान संज्ञौस्तः - अज्ञान के कारण संसार प्रतीत होता है। अज्ञानियों ने संसार मान करके ही तो बंध, मोक्ष का विकल्प किया है अर्थात् संसार और उसका बंध, मोक्ष अज्ञानियों की दृष्टि में है। परन्तु ऋतज्ञः कोऽर्थः आत्मज्ञः जो बोधवान आत्मनैष्ठिक महान पुरुष है उनकी दृष्टि इस संसार विकल्प का अभाव है और जब अचिन्त्य स्वस्वरूप भगवान आत्मा पर संसार नाम का विकल्प तीन काल में है ही नहीं तो फिर संसार का न बंध है और न मोक्ष है। कहते हैं कि आत्मदेश में संसार का बंध-मोक्ष किस प्रकार नहीं है? जैसे कि तरणी (सूर्य) में न अंधकार है-न प्रकाश, न दिन है- न रात। अब प्रश्न होता है कि सूर्य में अंधकार भले ही नहीं है, परन्तु प्रकाश तो है। तो कहते हैं कि जब अंधकार नहीं तो प्रकाश किसकी अपेक्षा से कहोगे? इसलिए सूर्य में न अंधकार है, न प्रकाश, न दिन है, न रात। इसी प्रकार जब विचार करो तो स्वस्वरूप भगवान आत्मा में न बंध है, न मोक्ष, न ज्ञान है, न अज्ञान। जब संसार ही नहीं है तो संसार का बंध कहाँ और अज्ञान कहाँ? जब बंध नहीं, तो मोक्ष कहाँ और अज्ञान नहीं, तो ज्ञान कहाँ?
अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात् ।
अजस्त्रचित्यात्मनि केवल परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ।।
त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मामेव च ।
आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोऽज्ञजनताज्ञता ।।
(10 - 14 - 27)
ब्रह्माजी कहते हैं- अहो महत् दुःखे, अहो इति खेदे। बड़े दुःख की बात है, तुझ सर्व के सर्व भगवान आत्मा को परं यानी दूसरा मानता है, अपने आपको साढ़े तीन हाथ का शरीर मानता है। अपने स्वरूप आत्मा से भिन्न मानता है कि परमात्मा भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। अनेक जन्मों से अनादिकाल से अज्ञानीजन तुम्हें पाने को बाहर-बाहर ढूँढ़ रहे हैं। अज्ञानियों की इस अज्ञानता को क्या कहें।
इसे सुनकर भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं-ब्रह्माजी तुम्हें बुढ़ापे में यह बीमारी कहाँ से पैदा हो गई कि नंद का बालक श्रीकृष्ण पाँच वर्ष की अवस्था में अघासुर दैत्य का वध कैसे किया? जाओ, तुम अपना सरकारी काम करो-अच्छा, अब जो बाल गोपाल और बछड़े ब्राह्मी गुफा में छुपाये हो, उन्हें प्रगट करो, ले आओ। मेरी इस लीला के चक्कर में मत पड़ो। इसके बाद भगवान ने काली नाग का अभिमान (दर्प) नष्ट किया और कंस द्वारा भेजे हुए अन्य दैत्यों का वध किया।
अब किसी समय हेमन्त ऋतु में ब्रजबालायें माता कात्यायनी का व्रत कर रही थीं।
हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दब्रजकुमारिकाः ।
चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चनव्रतम् ।।
(10 - 22 - 1)
हेमन्त ऋतु में (अगरह मास में) ब्रजमंडल की गोपकन्याएँ यमुनाजी के जल में सूर्योदय के पूर्व ही स्नान करके इस मंत्र का पाठ करते हुए माता कात्यायनी देवी का षोडशोपचार पूजन करती थी-
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि ।
नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः ।।
इति मंत्र जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः ।।
(10-22-4)
हे महामाये ! नंद बाबा के जो पुत्र श्रीकृष्ण हैं, वे हमको पति रूप में मिलें। नाम जपो, ध्यान करो, जो भी व्रत, दान करो, बात तो एक ही है। कोई व्रत करो, साधन करो, फल के लिए ही किया जाता है। तो इस मंत्र का पाठ करके ब्रज बालायें माता कात्यायनी देवी की पूजा करती रही। दिन में एक बार खीर का भोजन कर सारा दिन भगवान का गुणानुवाद करतीं। इस प्रकार एक मास का व्रत करती रहीं। अब आ गया परीक्षा का समय। यह चीरहरण का प्रसंग है। गोप बालायें कंठ भर जल में खड़ी होकर भगवान का गुणानुवाद गा रही थीं। इसी समय भगवान श्रीकृष्ण पुलिन पर पहुँचे और गोप बालाओं के वस्त्र को उठाकर कदम्ब के वृक्ष में टांग दिये और मन्द मन्द मुस्कुराते हुए गोप बालाओं को संबोधित करते हैं-
अत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम् ।
सत्यं ब्रवाणि नो नर्म ययूयं व्रततर्शिताः ।।
(10 - 22 - 10)
हे ब्रजबालाओं ! एक-एक करके सब आ जाओ और अपने-अपने पहन लो, वस्त्रों को ग्रहण कर लो। तुम इसे हँसी मजाक न मानो, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम लोगों का शरीर व्रत करते-करते कृश यानी दुर्बल हो गया है, जल्दी से शीघ्रतापूर्वक यमुना जल से निकलकर अपना-अपना वस्त्र धारण करो।
मानयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियम् ।
जानीमोऽङ्ग ब्रजश्लाध्यं देहि वासांसि वेपिताः ।।
श्यामसुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम् ।
देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद्राज्ञे ब्रुवामहे ।।
(10-22-14-15)
गोपियाँ कहती हैं कि हे श्यामसुंदर! हम सब गोपियाँ तुम्हारी दासी हैं। हे धर्मज्ञ ! धर्म के जानने वाले, वासांसि देहि हमें हमारे वस्त्रों को दीजिये और यदि तुम नहीं दोगे तो वयं राज्ञे कंसाय ब्रुवामहे हम लोग राजा कंस के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ नालिश करेंगी। भगवान कहते हैं कि जब तुम कहती हो कि तुम सब मेरी दासी हो तो जो मैं कहूँ वह तुम्हें करना चाहिये। भैया ! दशमस्कन्ध पूर्वार्द्ध के 22 vec q अध्याय का 26वाँ श्लोक है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-
न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते ।
भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ।।
(10-22-26)
ब्रजबालाओं ! जिसने अपने मन को मुझ आत्मा में प्रवेश कर दिया है, लीन कर दिया है, उसके मन में भी किसी प्रकार की कामना पैदा नहीं हो सकती। अरे ! जो दाना (धान का, मटर का या अन्य किसी अन्न का हो) एक बार जब आग में भुन जाता है तो उस दाने में फिर से अंकुर नहीं निकलते। इसी प्रकार जिसका मन रूपी दाना मुझ श्रीकृष्ण आत्मा रूपी प्रज्जवलित अग्नि में भुन गया है उसमें फिर काम की कामना कभी उत्पन्न नहीं होती। वासना रूपी अंकुर नहीं निकल सकता। देखो न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते- भगवान आत्मा में मन का भुनना क्या है? इसको समझो मानना किसका धर्म है, मन का कि आत्मा का ? अरे । जब कुछ न माना तो क्या रहा? मन का माना रहा या मन का मन रहा? देखो, भैया ! शिव बार-बार बतलाया जा चुका है कि मन का माना हुआ संसार है और सारी मान्यताओं का आधार 'मैं' आत्मा हूँ। ठीक ! यदि अपने मैं को कुछ मानो तो जैसा है वैसा ही है। तो 'मैं' का 'मैं' ही रहने दो। जो, जो है सोई रहने दो। 'मैं' को तुमने कुछ माना नहीं कि मन पैदा हो गया।
मन ने माना जगत को, मन को मान्यो आप ।
मन मिटते जग मिट गया, मुक्ता गुरु परताप ।।
(मुक्त दोहावली)
जी हाँ, तो समझो - 'मैं' को अछूता रखो। इस पर मान्यता न थोपो, 'मैं' को कुछ न मानो। 'मैं' को कुछ न मानना ही भगवान आत्मा के मन रूपी दाने का भुनना है। जब तक 'मैं' को कुछ मानते हो तभी तक साधन करने की इच्छा होती है। यह करूँ, वह करूँ, यह भाव रहता है। इस समय जितने भी बैठे हो, जो भी हो सब सद्गृहस्थ हो, साङ्गोपाङ्ग हो, परीक्षा करके देख सकते हो। जब तुम अपने को पुरुष मानते हो तभी तुम्हारे हृदय में स्त्री को देखकर कामवासना पैदा होती है। जहाँ तुमने अपने आपको पुरुष माना नहीं कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब पैदा हो गये। इसलिए अपने 'मैं' पर से पुरुष भाव हटा लो, तो तुम्हारे सामने कोई भी स्त्री चाहे स्वर्ग की अपसरा भी क्यों न आ जाये किसी की ताकत नहीं जो कि तुम्हें विचलित कर सके। इसी तरह प्रकृति समाज को कहना है कि अपने आपको जब स्त्री मानोगे तभी काम वासना पैदा होगी। अपने आपको स्त्री न मानो तो विश्व की ताकत नहीं जो तुम्हें विचलित कर सके। यह भगवद् वाक्य है, भगवान का वचन है। जब तक तुम्हारे मन में अमुक भाव नहीं रहेगा तो कभी कोई विकार मन में नहीं आयेगा। किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देख सके।
चलत मार अस हृदय विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा ।।
तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा ।।
कामदेव जब आया तो समझ गया कि बचना तो मुश्किल है। उसने पुष्प बाण ताना, बसन्त ऋतु निर्मित किया और काम विशिख बाण शिव को मारा। तो क्या हुआ? चितवत काम भयउ जरि छारा।। जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया। भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्या है? 'मैं' साक्षात् शिव हूँ-कल्याण स्वरूप जो भगवान आत्मा है वही साक्षात् शिव है।' मैं' हूँ मान्यता रहित, ऐसा जो विमल ज्ञान है, यही भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। जब भगवान शिव ने 'मैं' कल्याणस्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा देखा तो काम भस्म हो गया। कहते हैं कि भगवान शिव दिगम्बर है-लंगोटी भी नहीं लगाते- नंगे हैं, क्या मतलब? यही कि शुद्ध तत्व 'मैं' आत्मा अमुक भाव से रहित हूँ, विकल्प से रहित हूँ। यही भगवान शिव दिगम्बर हैं, इसका भाव है। अनन्त मान्यता रूपी मुंडों की मुंडमाला धारण किये हैं। सत, रज, तम तीनों गुण भगवान शिव का त्रिशूल है। 'मैं' आत्मा हूँ, यही भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। भगवान शिव के जटा से ब्रह्म विद्या रूपी विमल गंगा बह रही है। और अरे! जिस आत्मदेश में न प्रपंच है, न विकल्प है, परमशांतिमय स्थल है-यही श्मशान भूमि है। जहाँ पर मुर्दे ही जाते हैं, जिंदे नहीं। यहाँ अध्यात्म है। यहाँ श्रृंगार नहीं है। इसमें यदि श्रृंगार होता तो श्री शुकदेव स्वामी वैराग्य की साक्षात् मूर्ति वीतराग महात्मा राजा परीक्षित को यह कथा कैसे सुनाते और न उसका आत्म कल्याण ही होता। जो इस प्रसंग को श्रृंगार मानते हैं, उन्हें क्या कहें? यहाँ तो शुद्ध आत्मतत्व का विवेचन है। जी हाँ उनकी दोष दृष्टि कहें या क्या कहें-
न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते ।
भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ।।
हृदयाकाश ब्रजमंडल में चित्त की वृत्ति रूपी गोप कन्यायें मोक्ष की आशा रूपी कालिंदी में स्नान कर, निवृत्ति रूपी कात्यायनी देवी का व्रत करती थीं इसलिए कि श्रीकृष्ण भगवान आत्मा हमें पति मिलें अर्थात् हमें आत्मदर्शन, आत्मानुभव हो। भगवान श्रीकृष्ण आत्मा उन चित्त की वृत्ति रूपी स्त्री गोप कन्याओं को दर्शन देने के लिए मोक्ष के साधन रूपी सखाओं को लेकर यमुना तट पर पहुँचे और उनके वासना रूपी वस्त्रों को वैराग्य रूपी कदम्ब की शाखा पर टांग दिये। यही वस्त्राहरण आख्यान है। यह पूर्णतया आध्यात्मिक विषय है-
दासोऽहमिति या बुद्धिः श्रीकृष्णे मधुसूदने ।
दाकारोपहृतस्तेन गोपिकावस्त्रहारिणः ।।
चित्त की वृत्तिरूपी गोपबालाओं के हृदय में भगवान आत्मा श्रीकृष्ण के प्रति जो दासोऽहम भाव था उसमें 'दा' रूपी वस्त्र को भगवान ने हरण कर लिया। अब रह गया शुद्ध तत्व भगवान आत्मा 'मैं' का 'मैं' सोऽहम्, जो तू सोऽहम् (बोलो मुक्तेश्वर भगवान की जय-जय ध्वनि श्रोताओं द्वारा तुमुल जय-जयकार हुआ।)
यही चीरहरण अध्यात्म तत्व श्री परमहंस संहिता में वर्णित है? यह परमहंस संहिता है। पाठ के अन्त में यही आता है कि-इति श्रीमद्भाद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ।
-----------
पंचम दिवस :
दूसरी बेला
दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक
भगवान श्रीकृष्ण परमानंद विश्वात्मा की बाल लीला, दैत्यों का वध गोवर्धनोद्धारण, ब्रह्मस्तुति एवं चीरहरण के प्रसंग का उस समय वर्णन हो चुका है। यह सब चरित्र जब हो चुका तो महात्मा अक्रूर (कंस के प्रधानमंत्री) ब्रज आकर भगवान श्रीकृष्ण बलदेव को मथुरापुरी ले गये और वहाँ पहुँचने पर यदुवंशियों के नेत्रों के कण्टक कंस का वध इत्यादि हुआ। जब यह सब चरित्र हो चुका तो भगवान श्रीकृष्ण गुरु सन्दीपन के आश्रम में पढ़ने लगे और 64 दिन में 64 कलाओं-विद्याओं को पढ़कर गुरु के मरे हुए पुत्र को लाकर गुरु दक्षिणा में देकर अब वापस मथुरापुरी लौट आते हैं।
वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा ।
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः ।।
(10 - 46 - 1)
भगवान, एक दिन उद्धव जो कि साक्षात् वृहस्पतिजी के शिष्य बड़े बुद्धिमान्, भगवान श्रीकृष्ण के अंतरंग प्रिय सखा को एकान्त में बुलाकर कहते हैं-
गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रौ प्रीतिमावह ।
गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय ।।
(10-46-3)
भैया उद्धव ! तुम शीघ्र गोकुल को जाओ, जब से मैं यहाँ मथुरा आया हूँ तब से आज दिन तक गोकुल का कोई समाचार नहीं मिला है, इसलिए वहाँ जाओ, गोपियों को यह ज्ञान संदेश सुना देना। पता नहीं, मेरे वियोग में वे कैसे प्राणों की रक्षा कर रही होंगी। मेरे पूज्य पिता बाबा नंद, मैया यशोदा का कुशलक्षेम लाना, मेरा उन्हें प्रणाम कहना, क्योंकि उनका ध्यान, पूजन सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान श्रीकृष्ण के आदेशानुसार उद्धव गोकुल को रवाना हो गए। गोकुल पहुँचते-पहुँचते संध्या हो गई। उस समय गौएं जंगल से वापस आ रही hat pi गौओं के चरणों की धूलि से आकाश मंडल आच्छादित हो रहा था। जिसके कारण महाराज उद्धव को भ्रम हो गया कि बाबा नंद का घर कौन-सा हैं? देखते हैं कि वहाँ पर कहीं अग्निहोत्र हो रहा है, जगह-जगह भगवान श्रीकृष्ण की आरती, पूजन, यशोगान हो रहा है। भगवान की बाल लीला को राग, रागिनी में बद्ध कर उनके जितने सखागण हैं वे गा-गाकर नाच रहे हैं। ब्रज की ऐसी शोभा को देखते हुए महाराज उद्धव बाबा नंद के स्थान में पहुँचे। बाबा नंद अत्यन्त प्रेम भक्ति से उद्धव का स्वागत किये, मानो भगवान श्रीकृष्ण ही आये हैं। उनका स्वागत कर सत्कारपूर्वक अपने स्थान में ले आये।
तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियम् ।
नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत् ।।
( 46 - 14)
वसुदेवजी के मित्र बाबा नंद ने महाभाग्यवान उद्धव का स्वागत, स्नान, भोजन आदि कराकर उन्हें स्वस्थ किया और फिर उद्धवजी को ऊँचे आसन पर बिठाकर बाबा नंद और मैया यशोदा उन्हें घेरकर बैठ गये और भगवान का कुशल क्षेम पूछने लगे। अभी ब्रजवासियों को महाराज उद्धव के आने का पता नहीं लगा था। बाबा नंद महाराज उद्धव से पूछते हैं-
कच्चिदङ्ग महाभाग सखा नः शूरनन्दनः ।
आस्ते कुशल्यपत्याद्यैर्युक्तो मुक्तः सहृद्धृतः ।।
(10 - 46 - 16)
हे महाभाग उद्धव ! हमारे मित्र शूरसेन के पुत्र वसुदेव अपने पुत्रों भगवान श्रीकृष्ण एवं बलदेव सहित मथुरापुरी में आनंद से तो हैं?
अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन् ।
गोपान्व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् ।।
(10-46-18)
हे उद्धव ! क्या श्रीकृष्ण हम लोगों का, मेरा, अपनी माता यशोदा का कभी स्मरण करते हैं? माता यशोदा का ध्यान उन्हें आता है? अपने सखा गोप बालकों का ब्रजबालाओं का, कालिन्दी तट का, लीला भूमि का उन्हें कभी स्मरण होता है?
स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितम् ।
हसितं भाषितं चाङ्ग सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः ।।
(10-46-21)
हे अंग! हसितं भाषितं लीलापाङ्ग निरीक्षितम् च पुनः कृष्णवीर्याणि पराक्रमाणि यदा स्मरतां मया तदा सन् काले नः अस्माकम् सर्वाः क्रियाः शिथिला जाता। हे उद्धव ! भगवान श्रीकृष्ण के हँसने को, बोलने को, लीला भूमि को एवं उनके पराक्रम को जब मैं स्मरण करता हूँ, उस समय मेरी सारी क्रियाएँ शिथिल हो जाती हैं। भैया उद्धव ! श्रीकृष्ण जब मथुरापुरी गये तो कुलांगर दुष्ट कंस का वध हो गया। अब तो वहाँ पर बड़े ही आनंद में होंगे। कहते-कहते उन्हें लीला स्मरण हो आई और उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया। श्रीकृष्ण भगवान के ध्यान में निमग्न हो गये। वाणी अवरुद्ध हो गई। आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे-समाधिस्थ हो गये। बाद में मैया यशोदा भी प्रभु की लीला का स्मरण कर प्रेम विह्वल हो गई, स्तन से दूध टपकने लगा और समाधिस्थ हो गई। रह गये उद्धव जी-अब महाराज उद्धव कहते हैं-
युवां श्लाध्यतमौ नूनं देहिनामिह मानद ।
नायायणेऽखिलगुरौ यत्कृता मतिरीदृशी ।।
(10 - 46 - 30)
धन्य हो, बाबा नंद और माता यशोदे धन्य हो, अस्मिन् संसारे देहधारिणाम् नून् निश्चयेन युवां श्लाध्यतमौ, अखिल-गुरौ नारायणे इदृशी मतिः - संसार के अंदर देहधारियों में तुम दोनों धन्य हो। समस्त चराचर के गुरु नारायण में तुम दोनों की इस प्रकार की बुद्धि, ऐसी निष्ठा।
एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनी रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् ।
अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ ।।
(10-46-31)
जिन भगवान, श्रीकृष्ण एवं बलरामजी को तुम अपना पुत्र मानते हो, तुम्हारे भाग्य का क्या वर्णन करे- ये पुराण पुरुष हैं, विश्व के आधार हैं।
यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् ।
निर्हत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः ।।
(10-46-32)
यस्मिनं श्रीकृष्णचन्द्रे आत्मनि प्राणवियोगकाले मृत्युकाले विशुद्धं मनः क्षणं समावेश्य कर्माश्यं कर्मजालं निर्हत्य छित्वा आशु शीघ्रं अर्कवर्णः स्वयं प्रकाशः परां गतिं याति प्राप्नोति-जिन भगवान को आप अपना पुत्र मानते हो, वे कौन हैं? मृत्युकाल में जब प्राण का शरीर से वियोग होता है, उस वियोगकाल में जो क्षणभर के लिए भी भगवान आत्मा में विशुद्ध मन को प्रवेश करके प्राण त्यागता है, वह शीघ्र ही अनन्त जन्मों के कर्मजाल को काटकर परम गति, ब्रह्म पद, कैवल्य, निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है, उनको तुम अपना पुत्र मानते हो, आपके भाग्य की क्या सराहना करें-देहधारियों में सबसे अधिक भाग्यशाली हो, प्रशंसनीय हो। अब यहाँ प्रश्न होता है कि विशुद्ध मन किसको कहते हैं? और विशुद्ध मन का आत्मा में प्रवेश क्या है? यदि ऐसा कहो कि वासनाओं से रहित मन को विशुद्ध कहते हैं, तो वासनाओं से मन कदापि रहित नहीं हो सकता। कारण? मन वासनाओं का ही तो समूह है, पुञ्ज है, मन का अस्तित्व ही वासना है, तो फिर वह उससे रहित कैसे होगा। तो फिर विशुद्ध मन का क्या स्वरूप है? देखो, भैया ! मन कोई स्थूल पदार्थ तो है नहीं कि भगवान में उसको प्रवेश कर दिया जाय। अच्छा-विशुद्ध तो एक ही पदार्थ है, भगवान आत्मा। अब यदि मन को भी विशुद्ध कहो तो यहाँ पर वेदांत का द्वैतापत्ति दोष आता है। तो इसका भाव लगाओ। मान्यता ही वासना है। अच्छा-हाँ जी, समझो विषय- 'मैं' आत्मा पर जो मान्यता है (विकल्प है, अमुक भाव है) इसका ही नाम वासना है। जब मान्यतायें नहीं रहीं तो मन का अभाव हो गया केवल आधार 'अस्तित्व' मात्र रह गया। यही मन का आत्मा में प्रवेश होने का भाव है। सारी मान्यताओं के आधार भगवान आत्मा श्रीकृष्ण हैं। 'मैं' सारे विकल्पों का आधार हूँ, अमुक भाव भगवान आत्मा पर ही कल्पित हैं। तो मान्यताओं के अभाव का भाव ही विशुद्ध मन है। सूत्र लिखो- 'मान्यताओं के अभाव का भाव ही विशुद्ध मन है।'
यानी मान्यताओं का अभाव हो गया तो मन भी न रहा, क्योंकि वासनाओं के पुञ्ज का ही नाम तो मन है। कभी अपने आपको कुछ मानना, कभी कुछ मानना, यही वासनाओं का पुञ्ज है। मान्यता के अभाव के भाव का ही नाम विशुद्ध मन है। यही भगवान आत्मा में विशुद्ध मन का प्रवेश होना है। जब मान्यताओं का अभाव हो गया तो उस भाव में भगवान आत्मा ही आत्मा शेष रह जाता है, यही भगवान आत्मा में विशुद्ध मन का प्रवेश करना है तो-
यास्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् ।
निर्हत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः ।।
मान्यताओं का जब अभाव हो गया तो कर्मों की परिसमाप्ति हो गई। मान्यता जगत में जो शुभाशुभ कर्म हैं। कर्मजाल मान्यता जगत में ही है। आत्मजगत में नहीं। जब मान्यताओं का अभाव हो गया तो उसे विशुद्ध मन कहो या भगवान आत्मा कहो एक ही बात है। प्राण के वियोगकाल में यदि क्षण भर भी आत्मा में (आत्मा भावना में) स्थित होकर शरीर छोड़ता है तो अनेकानेक जन्मों के कर्मजाल को काटकर कैवल्य निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। उन्हें तुम अपना पुत्र मानते हो, क्या कहें आपके भाग्य को, देखो, अनुभव करो-अब कुछ मन के ऊपर भी सुन लो-
किस देश में मन अथवा मान्यता है? आत्मदेश में मन है कि मान्यता देश में मन है? मान्यता देश में मन है, आत्मदेश में नहीं। जब तुम अपने आपको कुछ मानते हो तभी मन दिखाई देता है। आत्मजिज्ञासुओं? लोग कहते हैं-मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मन की बीमारी संक्रामक है। इससे कोई अछूता नहीं। संसार के जीवमात्र सन्तप्त हैं। सभी रो रहे हैं। वही इससे बचता है-कौन? अरे ! जो हमेशा बचा हुआ है। जो इस मन से बचता है उसका क्या नाम है? भगवान आत्मा ! सिर्फ वही इस मन की बीमारी से बचा है। जीवभाव में कोई नहीं बच सकता। भैया! यह मन की बीमारी किस देश में फैली है? यह आत्मदेश की बीमारी है कि जीवदेश की? जीवदेश की बीमारी है। फिर लोग कहते हैं-स्वामी जी ! मन वश में नहीं होता-कितनी झूठ बात है-बोलो-बिना मन के वश में हुए कोई काम संसार में हो सकता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों का अनुभव क्या कभी भी बिना मन को वश में किये संभव है? नहीं, मन जब तक वश में न होगा विषयों का अनुभव नहीं हो सकता। मन की बेबसी में कथा सुन रहे हो कि मन के वश की हालत में कथा सुन रहे हो? झूठ न बोलो- मेरे कहने से न मानो-यदि मेरे कथन को उसी के अनुसार मान लेते हो तो यहाँ पर पंथ आ जाएगा। देखो-पंथ के गुरु चाहे किसी भी पंथ के हों, बैठे हैं और सेवकगण उनके चारों तरफ बैठे हैं-अब गुरुजी जो भी शब्द कहते हैं उसे सेवकगण सद्ववचन महाराज-कहते चले जाते हैं। यहाँ पर हम ऐसे नहीं मानते हैं, हर एक बात को सूक्ष्मता से समझो स्वयं अनुभव करो, जब तक न कर लो, न मानो। हम तुम्हें पचासों युक्तियों द्वारा समझायेंगे। यही हमारी ड्युटी है। जब समझ में आ जाये तब स्वीकार करो। अभी जो कथा सुन रहे हो, मन वश में है तब सुन रहे हो या मन की बेबसी में। संसार के जितने भी काम करते हो गद्दी में बैठे हो, लाखों रुपयों का हिसाब करते हो, रोकड़ लगाते हो, मजाल है कि एक पाई का भी फर्क हो जाये ये सब कार्य मन के वश में ही संभव है या बेबसी में? मन वश में है तब ये कार्य हो रहे हैं। जब ये कार्य मन के वश में तुम करते हो तो उस समय मन को वश में करने के लिए कौन-सा साधन करके बैठते हो? कौन-सी समाधि सिद्ध करके बैठते हो हिसाब लगाने या अन्य कार्य करने? आफिस में दिन भर काम करते हो तो कौन-सी समाधि सिद्ध करके बैठते हो? संसार में सारा काम मन के वश में करते हो, न कि बेबसी में। यह तुम्हारा झूठा दावा है कि मन तुम्हारे वश में नहीं है। जो भी कार्य करते हो मन हमेशा तुम्हारे वश में रहता है और तभी कोई भी कार्य कर सकते हो इसलिए यह झूठा मामला है। मन वश में नहीं होता-यह तुम्हारा मामला संतों की अदालत में खारिज किया गया। अच्छा-अब अनुभव करायेंगे-भैया ! वह कौन-सा टाइम है जब मन तुम्हारे वश में नहीं रहता-काबू के बाहर हो जाता है? जब पूजा में, पाठ में ध्यान-धारण में, आँख बंद करके बैठते हो तो उसी वक्त मन पैदा हो जाता है। दरअसल मन की पैदाइश इन्हीं समयों में होती है। अभी तो तुम सब अमनस्क पद में स्थित हो, कथा सुनते- सुनते झूम रहे हो-तुम जो भी कार्य करते हो सब स्वरूप स्थिति में करते हो। लोग कहते हैं कि स्वामीजी ! हमारी स्वरूप स्थिति नहीं हो रही है। भैया ! कैसे नहीं हो रही है? तुम सदैव स्वरूपस्थ हो। अभी जो कथा सुन रहे हो वह स्वरूपस्थिति में ही सुन रहे हो। अमनस्क पद में ही सुन रहे हो। मन के भाव में नहीं, मन के अभाव में सरा चराचर स्वरूपस्थिति में है।
सशान्त सर्वसंकल्पाः या शिलावदवस्थितिः ।
जाग्रन्निद्रा विनिर्मुक्त सा स्वरूपस्थिति परा ।।
यदा न लीयते चित्तं न विक्षिप्यते पुनः ।
अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ।।
(गौ.का.)
भाव दोनों का एक ही है। जिस समय चित का लय न हो और न चित्त विक्षिप्त हो (न लय, न विक्षेप) चित्त की चंचलता (विक्षेप) का नाम है जाग्रत अवस्था और चित्त के लय अवस्था का नाम है सुषुप्ति (गाढ़ी नींद)। वित्त न चंचल रहे और न ही विक्षिप्त रहे अर्थात् लय विक्षेप से रहित अवस्था ही आत्मपद कैवल्य पद निर्वाण पद है। 'जाग्रन्निद्रा निनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा'-जाग्रत और सुषुप्ति अवस्था से जो रहित अवस्था है वही स्वरूपस्थिति है। अब इसका अनुभव करो-समझ गये तो कल्याण हो गया। ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। सुनो-स्वरूपस्थिति, जाग्रत और सुषुप्ति इन दोनों से परे की अवस्था है। देखो-अभी जो कथा सुन रहे हो, इसे चित्त के लय. की अवस्था में सुन रहे हो या चित्त की चंचलता में सुन रहे हो, इसे चित्त के लय की अवस्था में सुन रहे हो या चित्त की चंचलता में सुन रहे हो? यार मीटिंग न करो, सोच-समझकर कहो कोई पहेली नहीं बुझा रहे हैं जो कि मीटिंग करो, समझकर बोलो-चित्त यदि लय हो जाये तो सुन नहीं सकते, नींद आ जायेगी और चित्त जब चंचल हो जाये तब भी नहीं सुन सकते-तो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए लय विक्षेप से रहित अवस्था में ही तो सुन रहे हो, यही स्वरूपस्थिति है। अब यह सिद्ध हुआ कि स्वरूपस्थ होकर ही समस्त विषयों का अनुभव करते हो। यदि स्वरूप से विलग हो तो सुन नहीं सकते और स्वरूप देश में मन नाम की कोई चीज ही नहीं, स्वरूप से भिन्न होने पर ही मन है। यही कारण है कि तुम्हारे पास अभी मन नहीं है। चाहे कोई बच्चा रोता हो, कोई जगह हल्ला होता हो तो मन नहीं जाता। अभी कथा सुन रहे हो-तो इस समय तुम्हारा मन विक्षेप की तरफ नहीं जाता। फर्ज करो कि यदि कथा के श्रवणकाल में मन कहीं चला जाता है तो तुम्हें ग्लानि नहीं होती और आ जाता है तो हर्ष नहीं होता। इसलिए यही स्वरूपस्थिति है। बिना स्वरूपस्थिति के किसी भी विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूति नहीं हो सकती- इसलिए सारा चराचर स्वरूपस्थ है। तो अब हमारी बात सुनो-अभी तक मन को रोकने का प्रयत्न करते थे, अब मन को न रोकने का प्रयत्न करो। अरे। अभी कहाँ मन को रोके हो, परन्तु मन रुका है तभी तो कथा सुन रहे हो? तुम अपनी महिमा को क्यों नहीं अनुभव करते, जैसे हो वैसे ही रहो-जहाँ हो वहीं रहो। 'मैं' जैसा हूँ वैसा ही हूँ, इस अवस्था में मन नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर दुःख अथवा सुख का अनुभव नहीं होगा। स्वामीजी ! कथा सुनने के समय तो मन रुका है, परन्तु यहाँ से जाने के बाद चंचल हो जाता है, इसे कैसे रोंके ? मन के रोकने का क्या साधन है? 'मैं' जैसा हूँ, वैसा ही हूँ, 'मैं' जो हूँ वही हूँ, 'मैं' जहाँ हूँ वहीं हूँ, इस अवस्था में मन है ही नहीं-यह निजानंद की मस्ती है। यही निर्वाणपद है। 'मैं' आत्मा कितना महान हूँ, यदि मुझे मन से भय लगे तो मैं आत्मा नहीं। अब समझ गये होगे। अब अपने मन के विषय में कोई शिकायत नहीं रही। मन का भाव किसमें माना, किसको माना, कहाँ माना? जिस वक्त पूजा-पाठ में बैठते हो उसी वक्त मन अपने आप पैदा हो जाता है। देखो, अनुभव करो-अभी कथा सुन रहे हो तो कथा के श्रवणकाल में अपने को कुछ मानकर कथा में बैठे हो या मैं अमुक हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा नाम अमुक है? कोई विकल्प (भाव) नहीं-जैसा हूँ, वैसा ही बैठा हूँ। 'मैं' जो हूँ वही होकर बैठा हूँ, जहाँ हूँ वही हूँ। इसी भाव में संसार के सारे व्यवहार होते रहते हैं। अब मन की चंचलता की शिकायत कहाँ? मान्यता ही मन है। दरअसल मन नाम की चीज पूजन-पाठ में ही दिखती है। माला लेकर बैठे हैं। हाथ गोमुखी में है, माला के दाने सड़सड़ चल रहे हैं, उसी समय मन पैदा हो जाता है। मजाल है कि मनीराम अन्य विषयों के अनुभवकाल में पैदा हो। स्वभावतः प्रत्येक विषय के अनुभवकाल में मन रुका रहता है, परन्तु ध्यान, धारणा में बैठे नहीं कि मन पैदा हो जाता है। पता नहीं इसका क्या कारण है। ध्यान, धारणा मान्यता जगत में प्रवेश करके ही करते हो। मैं जापक हूँ- इसलिए जप करूँ, मैं पुजारी हूँ-पूजा करूँ, मैं ध्यानी हूँ-ध्यान करूँ। पूजा- पाठ करने वाला ऐसा मानकर इन कार्यों में प्रविष्ट होता है और मानना ही मन का पैदा होना है। मानना ही मन है। जहाँ माना कि मैं जीव हूँ तो मन पैदा हो गया। भैया ! जब तक जीव भाव है तभी तक मन है। जहाँ माना कि मैं जीव हूँ तो मन पैदा हो गया। भैया ! जब तक जीव भाव है तभी तक मन है। अपने आपको संसारी जीव मानकर मन को वश में कर ले तो वन्ध्या का पुत्र सिंह का शिकार कर सकता है, निराधार आकाश में बगीचा लगाया जा सकता है. खरगोश के सींग हो सकते हैं, कछुवे की पीठ पर बाल जम सकते हैं, हथेली पर बाल उग सकते हैं, यब सब असंभव है। जीव भाव में मन को साधन से रोका जा सकता है, परन्तु मन को स्थिर नहीं किया जा सकता और आत्मभाव में मन को रोकने की जरूरत ही नहीं। महर्षि पतञ्जलि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से चित्त का निरोध बतलाते हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः । (योगदर्शन 1/2) चित्त के निरोध का नाम योग है। चित्त के निरोध के लिए साधन है, परन्तु चित्त के स्थिर करने के लिए नहीं। नदी स्वभावतः समुद्र में जाकर स्थिर हो जाती है, उसे कोई साधन नहीं करना पड़ता। हाँ-नदी को रोकने का बांध साधन अवश्य है। बांध से दिखता तो है कि नदी का प्रवाह रुका है, परन्तु वस्तुतः वह सदैव बांध को तोड़ने का कार्य करती रहती है और एक न एक दिन तोड़ भी देती है, परन्तु स्थिर तो समुद्र में जाकर ही होती है। इसी प्रकार मन है नदी, संकल्प विकल्प उसके दो किनारे हैं, साधन बांध है, कल्पना उसकी धार है। मन रूपी नदी साधन रूपी बांध से रूकी तो जान पड़ती है, परन्तु इस तरह साधन से स्थिर नहीं होती जहाँ की वह है वहीं पहुँचकर स्थिर होती है। आत्मदेश में पहुँचकर ही मन शांत होता है। जीवदेश में मन रोका जा सकता है, परन्तु आत्मदेश में स्थिर होता है। जीव को ही तो कुछ करने धरने का विकल्प होता है कि चलो भाई कुछ करें। जीव भाव में ही यह भावना होती है कि मेरा मन चंचल है, क्योंकि अनादिकाल से अपने को जीव ही तो मान रहा है कि मैं जीव हूँ, कर्ता-भोक्ता हूँ, धर्मी- अधर्मी हूँ, पुण्यी-पापी हूँ, ज्ञानी-अज्ञानी हूँ, जीता-मरता हूँ आदि। जीव अपने को संसारी मान कर इन धर्मों को अपने आप में आरोपित करता है। तो फिर इस भाव में मन चंचल रहेगा ही। सुषुप्ति अवस्था में अपने कारण अज्ञान में मन के लीन हो जाने पर फिर कोई भाव नहीं रहता। जब मन ही नहीं रहा तो भाव अभाव कहाँ। जब मन नहीं तो जीव भाव भी नहीं। जाग्रत, स्वप्न अवस्था तक ही मन है और तभी तक जीव भाव भी है। भैया ! बोध जगत में मन नाम की कोई चीज नहीं है-वहाँ मन कहाँ है। मन के भाव में जीवभाव है तो मन के अभाव में क्या यह जीवभाव रहेगा? मन कहो या जीव दोनों का भाव अथवा अर्थ एक ही है। जब मैं गाढ़ी नींद में सो जाता हूँ तो सबेरे उठकर कहता हूँ कि आज बड़ा आनंद आया, खूब सोया। सबेरे उठकर कौन बतलाता है कि मुझे बड़ा आनंद आया। इस अनुभव को कौन व्यक्त करता है। 'मैं' आत्मा ही इस आनंद का अनुभव करता हूँ। 'मैं' ही इसका साक्षी हूँ। 'मैं' जाग्रत के प्रपंच को जानता हूँ। 'मैं' ही स्वप्न के प्रपंच को जानता हूँ और 'मैं' ही सुषुप्ति के आनंद का भी अनुभव करता हूँ क्योंकि 'मैं' ही सर्वाधार हूँ सर्व का सर्व हूँ मुझसे विलग कोई नहीं। यह बात है !!!
एतावानात्मसम्मोहो यत् विकल्पस्तु केवले ।
आत्मन्नृते स्वमात्मानमवलम्बो न सयस्य हि ।।
(श्रीमद् भागवत 11)
बिना 'मैं' के और कौन आधार होगा? यह चीज ही ऐसी है। विकल्प अपने स्वरूप 'मैं' पर स्थित है।
जग में दुखिया कोई नहीं सबकी गठरी लाल ।
गाँठ खोल जानै नहीं ताते भयो कंगाल ।।
लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल ।
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल ।।
तो भैया ! अपनी महिमा को जानो। यहाँ कुछ लेना नहीं, लाना नहीं, न कुछ करना, धरना है। जहाँ जाना, वहीं खड़ा हूँ। जिसको देखना है, उस को देख रहा हूँ। जिसको पाना है, उसको पहिले से ही पाया हूँ। बस-जिस समय पूजा पाठ में मैं बैठता हूँ तो अपने आपको कुछ मान लेता हूँ और मानना ही मन है। तो पूजा करो या पाठ करो-टंट-घंट चाहे तो कुछ करना हो करो। हाँ-याद रखो कि यहाँ पर किसी बात का न खंडन होता है, न मंडन। इनका जो आधार है वह अध्यात्म है और उसी का निरूपण किया जा रहा है। सर्व व्यापक, सर्व के सर्व का निरूपण हो रहा है। वस्तुतः यही श्रेय है, आधार है, यहाँ द्वैत-अद्वैत किसी का निरूपण नहीं है और यहाँ पर न द्वैत का विरोध है न अद्वैत का, यदि अद्वैत का विरोध करें तो ब्रह्मवादी विरोध करेंगे और यदि द्वैत का विरोध करें तो जीववादियों का विरोध होगा। ऐसे विरोध को दूर से ही नमस्कार है। न यहाँ कोई राग है, न द्वेष। जिसमें राग-द्वेष है, उसे दूर से ही सलाम है। क्या उसे अध्यात्म निरूपण कहेंगे जहाँ कि राग-द्वेष है इसलिए इन सबको नमस्कार है। अब कौन इसमें विरोध करेगा-चाहे वह ईसाई हो या मुसलमान, चाहे कोई भी हो, इस सिद्धांत से किसी का भी विरोध नहीं है। विश्व में अपने आपको 'मैं' कौन नहीं कहता। चाहे वह किसी भी धर्म का हो-अपने आपको सभी 'मैं' मैं ही संबोधित करते हैं? यहाँ पर किसी की भी परवाह नहीं। चाहे कोई सगुण को भजे, चाहे निर्गुण को, परन्तु यहाँ तो किसी का भेद नहीं। यहाँ पर न सगुण का निरूपण है, न निर्गुण का। एकमात्र विशुद्ध तत्व का ही निरूपण हो रहा है। इसके लिए रामायण, श्रीमद् भागवत, गीता, उपनिषद् सभी साक्षी हैं। इनकी ही अध्यक्षता में इनके ही माध्यम से इन्ही के आधार पर इन्हीं के साक्षित्व में अध्यात्म का निरूपण हो रहा है। जान लो कि आत्मा क्या है? तो स्वामी जी ! पूजा, पाठ न करें? नहीं खूब करो, डटकर करो, अभी जितना करते हो उससे दुगुना-तिगुना करो-हम किसी का पूजा-पाठ क्यों छुड़ायें-हम तो यही कहेंगे कि भैया! इस तत्व को जान लो और फिर पूजा, पाठ डटकर करो। तुम अभी से अधिक शांति और आनंद का अनुभव करोगे। पूजा, पाठ तुम डटकर करो परन्तु समझ बूझकर। बात यह है कि देखा-देखी न करना, गुरुजी आँख मूंदते हैं तो हम भी आँख मूंदें, हम भी वैसा ही करें, ऐसा नहीं। देखा-देखी का एक दृष्टान्त सुना दें-
एक कथावाचक पंडित जी किसी दिन अपने यजमान के यहाँ कथा कहने गए। रास्ते में गंगाजी पार करना पड़ता था। कारण कि यजमान का स्थान गंगाजी के उस पार था, पंडितजी जब घर से निकले तो लोटा साथ में ले लिये। एक लोटा निस्तार के लिए और एक लोटा दाल बनाने के लिए। जब गंगाजी के किनारे पहुंचे तो सोचा कि चलो यहाँ से निवृत्त होकर स्नान आदि करके ही चलें। गंगाजी में स्नान, ध्यान, पूजा, पाठ करके जब निवृत्त हुए तो सोचने लगे यजमान के यहाँ दो लोटा लेकर जाने की क्या आवश्यकता है, यजमान के यहाँ खाना पकाने के लिए बर्तन तो मिल ही जाएंगे, तो नाहक लाये, लोटा भी लाये और कमरतोड़। यहाँ कौन देखता है, सब सूना है तो ऐसा करें एक लोटा यहीं रेत में गाड़ दें, वापस लौटने पर ले जाएंगे। तो गंगाजी के किनारे एक लोटा रेत हटाकर गाड़ दिया और निशानी के लिए एक रेत की पिण्डी उसके ऊपर बना दिया। कुछ दूर पर कुछ आदमी स्नान कर रहे थे, वे पंडित जी को लोटा दबाते तो नहीं देखे, परन्तु उन्होंने पिण्डी बनाते जरुर देखा। पंडित जी यजमान के घर चल दिये। जो लोग पंडित जी को पिण्डी बनाते देखे थे वे लोग गाँव में जाकर हल्ला कर दिये कि हम लोग अभी तक गंगा स्नान की वास्तविक क्रिया नहीं जानते। स्नान के बाद पिण्डी बनाना चाहिये तभी गंगा स्नान का फल मिलत ।है। पिण्डी बनाये बिना गंगा स्नान का पुण्य नहीं है। तो बाबूजी ! बालू तो मुफ्त का ही रहा-जितना चाहे पिण्डी बनाओ। वे 20-25 पिण्डी बनाते चले, जो स्नान करें, 10-15 पिण्डी बना दें, क्योंकि गाँव में मुनादी जो हो गई थी। तो यह बीमारी पिण्डी बनाने की गांव भर में फैल गई। सभी कोई पिण्डी बनावें। मीलों इर्द-गिर्द में हजारों की तादाद में पिण्डी वहाँ बन गई। जब पंडित जी एक महीने बाद यजमान के यहाँ से लौटे तो क्या देखते हैं कि वहाँ तो हजारों पिण्डी बने हैं। अब लोटे का पता कैसे लगावें कि उनका लोटा कहाँ दबा पड़ा है। दो-चार जगह खोजे, परन्तु जब लोटे का पता न लगा तो वहीं पर पंडित जी ने एक श्लोक बनाया।
गतानुगतिको लोका न लोकाः पारमार्थिकाः ।
बालुका पिण्डदानेन गतं मे ताम्रभाजनम् ।।
संसार वास्तविकता को नहीं देखता, देखा देखी करता है। मैंने पिण्डी क्या बनाया, मेरा लोटा ही गायब हो गया।
हानि-लाभ कुछ न समझकर चलेंगे भेडिया धसान। जप करना चाहिये, लगाये ध्यान और आँख मूंदकर बैठ गये। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे कहने से ही न मान लो, पहिले समझ लो नहीं तो यही देखा-देखी की दशा होगी और बिना जाने कुछ करने कराने से ही मन पैदा होता है इसलिए ऐसा करो जैसा अभी कर रहे हो, नहीं तो फिर जैसे ही दोनों आँखें मूंदे वैसे ही मन तंग करेगा और स्वभाव में मन तंग न करेगा। इसी तरह से पूजन-पाठ करो, कुछ बनो मत, जैसे हो वैसे ही रहो। यहाँ पर हम आपके मन पर मुरादाबादी गिल्ट करने नहीं आये हैं। अपने आप मुसीबतों को झेलकर अनुभव करके फिर बता रहे हैं। मन पैदा करना है तो मन काबू करने के लिए साधन रूपी बांध बनाओ। यह ठिकाने की बात है और यही हम तुमको बता रहे हैं जो रूपी रहे हैं शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं जो कि बता स्वयं अनुभव किया है। कष्ट करके, हिमालय की गुफा में रहकर, जंगलों में भटककर, नाना प्रकार के कष्टों को सहकर, गंगाजी के किनारे तपस्या करके, हमारे पास एक झोपड़ी भी नहीं है, जो मिला पा लिये, जैसा पहना दिये पहन लिये और नाना प्रकार के आश्रमों में भटककर जो देखा, समझा, अनुभव किया वही आपको बता रहे हैं। हम अपनी पूंजी से देने आये हैं। दान दो प्रकार के होते हैं-जब वृद्धावस्था आ जाती है तो कुछ लोग वानप्रस्थ ले लेते हैं और हृषीकेश में गंगा के किनारे कमंडल लेकर, एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। उनके मन में जो पूर्व कर्मों की छाप पड़ी है, वहाँ भी वही करते रहते हैं। ऐसे जो मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी वानप्रस्थी हैं दो-चार महीने में पंजाबी पंजाब को, मारवाड़ी मारवाड़ को, गुजराती गुजरात को चले जाते हैं और 10-15 हजार चंदा जुटा लेते हैं। उसमें से कुछ वहाँ के क्षेत्र में दे देते हैं, कम्बल बांट देते हैं और बाकी से अपना खर्च चलाते हैं और कुछ दानी कलकत्ता, मुम्बई से जो धनी-मानी बड़े आदमी आते हैं वे किसी से कुछ पैसा नहीं लेते वरन् स्वयं की कमाई का धन लगाकर क्षेत्रों में दान कर देते हैं। इसी प्रकार जो उपदेशक शास्त्रों से चंदा लेकर उपदेश करते हैं वे दूसरे की कमाई में से दान देने वाले हैं और हम अपनी कमाई (अपनी पूंजी) से देते हैं। स्वयं अनुभव करके फिर बतलाते हैं। स्वयं अनुभव किये कि कब मन पैदा होता है, क्यों होता है आदि, क्योंकि हमें आपसे कोई निहोरा (एहसान) नहीं है। हमें एक तिनका भी नहीं चाहिये। हमारे पास तो एक घास की झोपड़ी भी नहीं, न बैठने को स्थान-जो कुछ कमण्डल, कपड़े रहे भी तो उसे साधु लोग ले जाते हैं। अब जो पहना दो वह पहन लेते हैं, जो खिला दिया पा लिये और यही रात-दिन का परिश्रम, बड़ी-बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। यह सब हम स्वभाव से कह रहे हैं। यह हमने स्वयं अनुभव किया है कि किस वक्त मन रहता है और कब नहीं रहता-ये सब प्रमाणयुक्त बाते हैं। पुराणों की अध्यक्षता में बतला रहे हैं। रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत, उपनिषदों की अध्यक्षता में-इनका प्रमाण ले लेकर, अनुभव लेकर तुम्हें इसका अनुभव करा रहे हैं। हाँ, जी-
यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् ।
निर्हत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः ।।
(10-46-32)
जो महाभाग उद्धवजी मैया यशोदा और बाबा नंद की सराहना कर रहे है कि धन्य है आप लोगों के भाग्य कि ऐसे भगवान श्रीकृष्ण को तुम अपना पुत्र मानते हो। जिसमें, विशुद्ध मन को प्राण के प्रयाण काल में प्रवेश करने से संसारी जीव कर्मजाल से छूट जाता है, उन्हें तुम अपना पुत्र मानते हो, धन्य हो तुम्हें-
तस्मिन्भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्ती ।
भावं विधत्तां नितरां महात्मन्किंवावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम् ।।
(श्रीमद् भागवत 10-46-33)
भगवान आप लोगों को अवश्य दर्शन देंगे। वे कहीं नहीं गये हैं, ब्रजमंडल सूना नहीं हुआ है-वे तो विश्वात्मा हैं, चराचर के अस्तित्व हैं, उनसे न किसी का संयोग होता है, न वियोग। न उनके कोई माता हैं न पिता, न स्त्री, न पुत्र। जिस प्रकार लकड़ी से डंडे का कभी संयोग-वियोग नहीं होता, इसी प्रकार भगवान आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जिससे किसी का न संयोग होता है, न वियोग होता है। क्योंकि आत्मा सर्व का सर्व है समस्त चराचर का अस्तित्व है, विश्वधार, सबका प्रकाशक भगवान आत्मा ही है और बाकी सब में 420 है, बाकी सब में धोखा है-समझ लो कान खोलकर-
नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् ।
अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमवलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्मेकात्मप्रत्ययसारं
प्रपंचोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ।।
(माण्डू. गौ.का. आगम प्र. 7)
यहाँ पर भगवान आत्मा के विशेषण दर्शाये गये हैं। इनमें एक विशेषण भगवान के लिए आता है प्रत्ययसार-अब इसका हम विवेचन करेंगे। प्रत्ययसार का उपनिषदों में अर्थ होता है विश्वसनीय पदार्थ-जिसका विश्वास किया जा सके। देखो, कभी किसी को आवेदन पत्र लिखना है यानी एप्लीकेशन देना है, तो आवेदक अपना आवेदन पत्र लिखता या टाइप कराता है। जब वह आवेदन पत्र पूरा लिख लेता है तो नीचे लिखता है, यदि अंग्रेजी में लिखा है तो युवर्स कैथफूली और यदि हिन्दी में लिखा है तो तुम्हारा विश्वासपात्र समझो विषय- भैया ! विश्वासपात्र क्या है? क्या यह शरीर विश्वासपात्र है, जिसका ठिकाना ही नहीं कि कब साथ छोड़ दे? क्या ये इन्द्रियाँ विश्वसनीय हैं? पता नहीं, आँख खुली है वह खुली ही रह जाये, बन्द न हो-कान कब बहरे हो जायें, क्या हाथ, पैर विश्वसनीय हैं? कब टूट जायें, अपंग हो जायें, तो फिर विश्वसनीय क्या है? क्या प्रमाण है कि जो सांस बाहर गई है वह अंदर आयेगी कि नहीं? अंदर न आये तो प्राण भी विश्वसनीय नहीं है-क्या मन विश्वसनीय है? यदि कहो कि मन के ऊपर विश्वास करना चाहिए तो यह कभी अच्छे में और कभी बुरे में जाता है, कभी स्थिर तो कभी चंचल हो जाता है, तो मन भी विश्वसनीय नहीं है। विश्वास करने लायक न तो शरीर, न इन्द्रियाँ, न प्राण, न मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कोई भी नहीं है। तुम जो लिखते हो कि तुम्हारा विश्वसनीय (युवर्स फैथफुली) तो फिर वह विश्वसनीय कौन है? किसके लिए लिखते हो 'तुम्हारा विश्वासपात्र'? नीचे लिखते हो 'मैं' और फिर पूँछ लगा देते हो कि शरद कुमार, प्रतापचन्द्र, मनोहरलाल या टेटकू खचेडू आदि। अरे ! हाँ- मजाल है कि 'मैं' में पूँछ न लगे तो चाहे जो लगा दो, परन्तु असली विश्वासपात्र तो 'मैं' आत्मा ही हूँ, बाकी सब में धोखा है। सब चीज की तो टाइप होती है, परन्तु क्या 'मैं' की भी टाइप होती है? भैया ! यह एक व्यवहारिक वेदांत है। मैं आत्मा की कभी टाइप नहीं होती। मैं आत्मा तो सबकी टाइप करता हूँ, मुझ आत्मा की टाइप कौन कर सकता है? मुझ आत्मा का टाइप करना क्या है? यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह बालक-युवा, वृद्ध है, मकान, वृक्ष, जड़, चेतन सब खड़े हैं, सब जानना ही मुझ आत्मा का टाइप करना है। क्या भगवान स्वयं अपनी टाइप करता है? प्रपंच की टाइप होती है। सुषुप्ति के आनंद का मैं आत्मा टाइप करता हूँ। मूर्छा एवं समाधि का टाइप मैं आत्मा करता हूँ। अस्पताल में किसी का आपरेशन होता है, तीन घंटे तक वह बेहोश रहता है, बाद में होश आने परवह कहता है-मैं तीन घंटे बेहोश रहा। अब प्रश्न होता है कि जब उसको होश ही नहीं था तो उस बेहोशी का अनुभव किसने किया? उस बेहोशी को किसने जाना? होशी और बेहोशी का अनुभव क्या मन करता है? अरे! मन ही तो तीन घंटे तक बेहोश रहा। इस बेहोशी का अनुभव 'मैं' आत्मा करता हूँ। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था में, भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों काल में 'मैं' आत्मा एक रस रहता हूँ। मुझ आत्मा के सिवाय और क्या विशेष (जानने लायक) है? इसलिए 'मैं' आत्मा ही विश्वासपात्र हूँ। टाइप जब पूरा हो जाता है तो मैं का दस्तखत (सही) मैं ही करता हूँ या कोई दूसरा कर देता है? 'मैं' का लेखक 'मैं' खुद ही हूँ, दूसरा नहीं लिख सकता। यहाँ पर सब पढ़े-लिखे लोग बैठे हैं, यदि दूसरा लिखे तो क्या होगा? जुर्म लगेगा। 'मैं' का लेखक दूसरा नहीं। 'मैं' ही हूँ। 'मैं' का टाइप 'मैं' ही करता हूँ। फर्ज करो जो पढ़ा-लिखा नहीं है तो अंगूठे की निशानी भी उसी की लगेगी। यह 'बात' संसार में यह विलक्षण व्यवहारिक वेदांत है। 'मैं' के सिवाय सबमें 420 है, धोखा है, इनसे बचो। भगवान आत्मा जो सर्व का सर्व है उसी का निरूपण हो रहा है। मजा आ गया-हाँ जी, बेछनी छन रही है भैया-
हाँ तो महाराज उद्धव बाबा नंद और मैया यशोदा को समझा रहे हैं। क्या आप लोग यह समझते हैं कि भगवान यहाँ से चले गए और ब्रजमंडल सूना हो गया-
न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः ।
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ।।
(10 - 46 - 38)
उनके न कोई माता हैं, न पिता, न पत्नी, न पुत्रादिक, न अपना है, न पराया, न देह है, न जन्म, न लीला, न स्तुति, न चरित्र, परन्तु भगवान आत्मा में इन सबकी मान्यता है।
तमेव शरणंगच्छ सर्वभावेन भारत ।।
(गीता)
सर्वभाव से उसकी ही शरण में जाओ, भगवान आत्मा ही एक ऐसा तत्व है कि जिसमें सर्वभाव घटित होते हैं, अन्य में नहीं।
दृष्टं श्रुतं भूत भवद् भविष्यद् स्थानस्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च ।
विनाच्युताद् वस्तु तरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थ भूतः ।।
(10 - 46 - 43)
आज के पहिले जो कुछ देखा था, सुना था और जो कुछ था, आगे जो कुछ देखोगे, सुनोगे और रहेगा, अभी जो कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो और है, स्थावर जंगम सब कुछ भगवान है अच्युत भगवान आत्मा श्रीकृष्ण से भिन्न एक तृण भी नहीं है। यही परमार्थ का स्वरूप है।
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ।।
(माण्डू गो.का.वै.प्र. 32)
दृष्टं श्रुतं भूत भवद्भविष्यत्स्थास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च ।
विनाच्युताद्वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः ।।
(10-46-43)
एवं निशा सा ब्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् ।
गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्वास्तून्समभ्यर्च्य दधीन्यमन्थन् ।।
(श्रीमद् भा. 10-46-44)
हे राजन परीक्षित् ! इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण का गुणानुवाद गाते, बोलते बाबा नंद, मैया यशोदा और उद्धव जी की रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः बेला में उद्धव कमण्डल लेकर कालिंदी स्नान के लिए चल पड़े। तो रास्ते में क्या देखते हैं कि-
एवं निशा सा ब्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् ।
गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्वास्तून्समभ्यर्च्य दधीन्यमन्थन् ।।
गोपियां उठ बैठी हैं और दीपक जला-जलाकर दही मन्थन करने लगी है। साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की लीला का गायन कर रही है, यशोगान कर रही हैं।
ता दीपदीप्तैर्मणिभिविरेजू रज्जूर्विकर्षद्भुजकङ्कणस्रजः ।
चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डलत्विषत्कपोलारुणकुङ्कमाननाः ।।
(10 - 46 - 45)
दीप जलाकर दही मन्थन कर रही थीं तो उनकी चूड़ियों में दीप की लौ पड़ने से एक विलक्षण शोभा (प्रतिभा) दिखलायी दे रही थी।
उद्गायतीनामरविन्दलोचनं ब्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशद्ध्वनिः ।
दघ्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्गलम् ।।
(10-46-46)
तो कहते हैं कि खाली दही मन्धन हो रहा है वहाँ पर या और कुछ हो रहा है? गोपियाँ दही मन्थन करती हुई भगवान के गुणानुवाद का गायन कर रही हैं, जिससे दशों दिशायें मंगलमय हो रही हैं। ऐसी प्रातःकालीन शोभा को देखते हुए महाराज उद्धव कालिन्दी स्नान को चले गये और इधर भगवान भुवन भास्कर उदय हो गये। गोपियाँ नन्दबाबा के भवन के सामने क्या देखती हैं कि उनके द्वार पर एक सुंदर रथ खड़ा है। रथ को देखकर वे आपस में तर्क करती हैं-ऐ सखी! देखो तो यह रथ कहाँ से आया है?
अक्रूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः ।
येन नीतो मुधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः ।।
(10-46-48)
यह किसका रथ है? कहाँ से आया है। दुष्ट कंस के अर्थ को सिद्ध करने अक्रूर तो फिर से नहीं आया है जो कि हमारे परम प्रिय कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण को मधुरापुरी ले गया है।
शुचिस्मिताः कोऽयमपीच्यदर्शनः कुतश्च कस्याच्युतवेषभूषणः ।
इति स्म सर्वाः परिववुरुत्सुकास्तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम् ।।
(10-47-2)
जिस समय गोपियां इस प्रकार तर्क कर रही हैं, उसी समय महाराज उद्धव स्नान संध्या से निवृत होकर बाबा नंद भवन की ओर सीधे चले आ रहे हैं। गोपियाँ कह रही हैं-मालूम होता है कि मथुरापुरी से आया है। भगवान श्रीकृष्ण के ही समान वेश है। वैसे ही पीताम्बर किरीट, मुकुट धारण किया है। उनका ही सेवक जान पड़ता है। उन्होंने ही भेजा होगा। गोपियाँ ऐसा कह रही थीं कि महाराज उद्धव वहाँ पर पहुँच गये। गोपियों ने उन्हें रोक लिया, बाबा नंद के सदन तक न जाने दिया। एक चौकी लाकर उसमें महाराज उद्धव को सत्कारपूर्वक बिठाकर ब्रजबालाएं चारों तरफ से उन्हें घेर कर बैठ गई। आइये, पधारिये आपका स्वागत है। आप भगवान श्रीकृष्ण के सखा हैं, मथुरापुरी से आए हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है-हाँ, श्रीकृष्ण भगवान भेजे होंगे, अपने माता-पिता की सुधि आ गई होगी तो उनके लिए संदेश भेजे होंगे-
अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे ।
स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरहि सुदुस्त्यजः ।।
(10 - 47 - 5)
अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम् ।
पुम्भिः स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्स्विव षट्पदैः ।।
(10 - 47 - 6)
अपने माता-पिता, बन्धुओं का कुशलक्षेम पूछने भेजे होंगे-नहीं तो हम ब्रज की गोपियों को भगवान श्रीकृष्ण क्यों पूछने चलेंगे। श्रीकृष्ण भगवान तो हम लोगों को ऐसे छोड़कर चले गये कि-
निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः ।
अधीतविद्या आचार्यमृत्विजो दत्तदक्षिणम् ।।
(10-47-7)
प्रजा अपने निर्धन राजा को छोड़ देती है, वेश्या धनहीन प्रियतम को छोड़ देती है। भैया ! संसार में इस प्रकार भगवान को भक्त ही कह सकते हैं। भक्त ईश्वर को भी कहने में नहीं चूकते। एकता जिसमें हो वही ऐसा कह सकता है। इतनी धृष्टता, जिसके लिए कोई विकल्प नहीं ऐसे भगवान की तुलना यहाँ पर गोपियाँ वेश्या से कर रही हैं और फिर कैसे छोड़कर चले गये? जैसे कि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा तब तक करता है जब तक कि उसे विद्या प्राप्त नहीं हुई। जब पढ़कर निकलता है तो फिर बाद में गुरुजी के प्रणाम भी करने नहीं जाता। विद्यार्थी आचार्य का परित्याग कर देता है। पुरोहित यजमान के यहाँ पूजा-पाठ कराता है और जब दान दक्षिणा मिल गई तो फिर यजमान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। फिर चाहे यजमान जाय जहन्नुम में। वैसे ही हमारे श्रीकृष्ण भगवान हैं-अब पता नहीं, वे आते हैं कि नहीं। ये सब बातें महाराज उद्धव को घेरकर गोपियाँ आपस में कह रही थीं और उद्धव चुपचाप सुन रहे थे कि इसी समय कहीं से एक भौंरा उड़ते हुए आया और किसी गोपी के चरण पर बैठ गया। नाम तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, परन्तु विद्वानों का अनुमान है कि वह महारानी राधिका जी ही थीं। भाव यहाँ पर यही है। गोपी के नाम से राधिका जी का ही संबोधन है। भौरा गोपी के चरण में आकर बैठ गया। अब उद्धव जी की शामत आ गई। गोपियाँ भौर के माध्यम से श्रीकृष्ण के प्रति कहती हुई उद्धव जी को फटकारने लगीं उन्हें इसका बहाना मिल गया। भौरे की तरफ मुखातिब (सन्मुख) होकर कहती हैं-
मधुप कितवबन्धो मा स्पृशानि सपत्याः ।
कुचविलुलितमालाकुंकुमश्मश्रुभिर्नः ।।
(10-47-12)
वहत् मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं ।
यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् ।।
(10-47-12)
हे मधुप, हे भ्रमर, अरे कपटी के दूत। तू मथुरापुरी से आया है? श्रीकृष्ण का समाचार लेकर ये संबोधन गोपियाँ भ्रमर की तरफ इशारा करके कह रही हैं। तू मेरे चरणों को स्पर्श न कर-संसार में भोली-भाली लक्ष्मी ही एक ऐसी स्त्री है जो कि भगवान श्रीकृष्ण की सदैव चरण सेवा करती रहती हैं। पता नहीं, लक्ष्मी को ऐसे धोखेबाज से क्या मोह है, जो कि सदैव उनके चरणों की सेवा में रत् रहती है। अरे भ्रमर, जैसे श्रीकृष्ण कपटी हैं, ऐसे ही तू भी कपटी है-
मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा ।
स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम् ।।
(10-47-17)
बलिमपि बलिमत्त्वाऽवेष्टयद् ध्वांक्ष्वद् यस्तदलम ।
सितसख्यैर्दुस्त्य जस्त त्कथार्थः ।।
भगवान के जन्म की क्या कहें, हमारे पास तो उनके तीन-तीन जन्मों का रिकार्ड है। उनके ऐसे कपट कर्मों का तीन युग का इतिहास हमारे पास है। सतयुग में जब तेरे स्वामी श्रीकृष्ण ने वामनावतार लिया तो पहुँच गए राजा बलि के पास। राजा बलि यज्ञ कर रहा था। भगवान वामन पहुँचे और बलि से दान में तीन पग पृथ्वी मांगे। मांगते समय तो थे बावन अंगुल के और नापते समय हो गये आकाश, पाताल। दो ही पग में समस्त लोकों को नापकर तीसरे पग के लिए उसे ऋणी बना दिया और उसे पाताल लोक में भेज दिया। यह सरासर धोखा नहीं तो और क्या है? त्रेतायुग में भी देख लिया-एक भाई सुग्रीव से मित्रता की और दूसरे भाई बाली को पेड़ की आड़ में छिपकर मारा। हाँ- सामने होते तो मालूम पड़ जाता और पंचवटी में बेचारी सूर्पणखा भगवान राम के पास आई। भैया। इनमें बड़ी एकता है। हाँ। वैसे आपस में भले ही झगड़ें, परन्तु बाहरी आक्रमण यदि इन पर हो तो फिर ये चण्डी ही हैं, न छोड़ेंगी। सब एक हो जायेंगी। मान लो कि तुमने अपनी स्त्री को एक तमाचा मार दिया, हम यह नहीं कहते कि तुम जाकर अब अपने यहाँ तमाचा ही लगा देना, परन्तु ऐसा मौका आ गया, कभी न कभी आ ही जाता है, तो भैया। ये सब पास-पड़ोस की जितनी स्त्रियाँ हैं सब एक हो जाएंगी, सब की सब औरतें तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी-बेचारी को नाहक मार दिया, निर्दयी है, अपनी औरत को क्यों मारा- इनमें बड़ी एकता है-तो बेचारी सूर्पणखा श्रीराम के पास मोहित होकर आई और क्या कहती है-
तुम सम पुरुष न मो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी ।।
तुम्हारे समान सुंदर पुरुष नहीं और मेरे समान स्त्री नहीं, इस पद के दो अर्थ हैं-ऊपर के चरण में सुंदरता का वर्णन है और दूसरे चरण में संयोग का वर्णन है। तो भगवान राम क्या कहते हैं-
सीतहि चितई कही प्रभु बाता। अहइ कुमार मोर लघु भ्राता ।।
यदि तू सुंदरता के लिए कहती है तो सीतहि देख, उसके चरणों की धूलि के समान भी तू सुंदर नहीं है और यदि संयोग यानी ब्याह के लिए कहती है तो भी सीतहि देख, मेरे पास सीताजी हैं और मैं एक नारीव्रती हूँ-हाँ लक्ष्मण अकेला है, उसके पास कोई नहीं है, तू वहाँ जा। बेचारी सूर्पणखा झांसेपट्टी में आ गई। सरकार के कहने से लक्ष्मण के पास गई और सरकार इधर लक्ष्मण को इशारा कर दिये, नाक-कान बिनु कीन्ह बिना नाक, कान के कर दिये, नक्टी-बूची कर दिये। इसलिए, अरे भ्रमर ! तू कपटी का सखा है और तू भी कपटी है। ऐ भ्रमर ! क्या तू चरण छूकर मनाने आया है? जा, जा, चला जा-तेरे द्वारा हम लोग भुलावे में आने वाले नहीं हैं। अरे भ्रमर ! यदि तू ऐसा कह कि गोपियों ! जब तुम लोग श्रीकृष्ण को ऐसे धोखेबाज हैं करके जानती हो तो फिर उनका नाम छोड़ दो, उनकी चर्चा छोड़ दो, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो जो कि उस धोखेबाज के विरह में, उनकी विरह व्यथा से क्यों संतप्त हो, जल रही हो, यदि तू ऐसा कह तो हम क्या करें हम सब विवश हैं, मजबूर हैं-
यदनुचरितलीला कर्णपीयूषविपुट्सकृददनविधूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टाः ।
सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीनाबहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति ।।
(श्रीमद् भागवत 10-47-18)
(पू. श्री स्वामी जी इस श्लोक के पाठ में गला रूँध गया, आँखें प्रेमाश्रु से भर आई, ध्यानमग्न हो गये, भाव समाधि में समाधिस्थ हो गये) 'शिव' एक बार भी जो अपने मानव जीवन में, अपने दोनों कानों द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के लीलामृत का पान कर लेता है और वह चरितामृत जब उसके हृदय देश में पहुँचता है तो उसके द्वन्द्वादिक विकार (धर्म) नष्ट हो जाते हैं। फिर वह सपदि माने शीघ्र ही घर-बार, स्त्री-पुत्र, कुटुम्ब, अपना पराया, जाति, आश्रम सब प्रकार के व्यक्तित्व का परित्याग कर नाम, रूप की मान्यता को छोड़कर संसार से उदासीन होकर कफन की लंगोटी लगाये उन्मत्त की भांति भ्रमता रहता है। वासुदेवः सर्वमिति-यानी समस्त चराचर को अपना स्वस्वरूप आत्मा देखता हुआ, आत्मदर्शी होकर घर-घर का टुकड़ा मांगकर खाता है और निराधार आकाश मंडल में जिस प्रकार पक्षी उड़ता है, उसी प्रकार निराश्रय होकर इस पृथ्वी मंडल पर विचरण करता है। एक बार भी, जो उनके लीलामृत को पी लेता है (पू. श्री स्वामी जी का गला रुंध जाता है)
उसकी यह हालत हो जाती है, तो फिर हम लोग जो 11-11 वर्ष उनके साथ रही हैं। श्रीमद् भागवत में तो नहीं परन्तु गर्ग संहिता में इसका प्रमाण आता है कि श्रीकृष्ण भगवान ग्यारह वर्ष गोकुल में रहे सौ वर्ष मथुरा में और पच्चीस वर्ष द्वारिकापुरी में। इस तरह कुल एक सौ छत्तीस वर्ष इस पृथ्वी मंडल पर रहकर लीलाएं की हैं। गोपियां प्रेम से विह्वल हो गई और कहती हैं कि जानते हैं श्रीकृष्ण भगवान 420 हैं, ऐसे धोखेबाज हैं, परन्तु क्या करें, जी भरकर उनका चरितामृत पान किया है, उनके वियोग में हम सब मर रही हैं और मरेंगी जीवन भर। इसी समय भौंरा अन्यत्र उड़ गया, तो प्रसंग ही खतम हो गया। अब महाराज उद्धव को बोलने का समय मिला। तो कहते हैं-
अहो यूयं स्म पूर्णार्धा भवत्यो लोकपूजिताः ।
वासुदेवे भगवति यासामित्यर्पितं मनः ।।
(10-47-23)
अहो ब्रजबालाओं । तुम लोग धन्य हो, लोक में पूज्य हो, तुम्हें क्या कहें, धन्य हो, भगवान वासुदेव में तुम लोगों का ऐसा अनन्य प्रेम हो, इतनी अगाध भक्ति है। यह प्रेमलक्षणा तो मुनीनामपि दुर्लभा मुनियों को भी दुर्लभ है। बज बालाओं ! मैं तुम लोगों के लिए भगवान श्रीकृष्ण द्वारा भेजा हुआ कर कमलोकित संदेश लाया हूँ। प्रभु का यह प्रिय संदेश तुम सब ध्यान से सुनो-
श्रूयतां प्रियसंदेशो भवतीनां सुखावहः ।
यमादायागतो भगा अहे भूर्त रहस्करः ।।
(10-47-28)
प्रिय संदेशः - प्रियस्य संदेशः प्रिय संदेशः । प्रिय का जो संदेश उसे कहते हैं प्रिय संदेश। अरे! जो सारे विश्व की आत्मा है-गोपियों का जो प्रिय है, जो सारे चराचर का प्रिय है, जो सर्व का सर्व है, सर्व का आनंद देने वाला है। चाहे कोई भी हो एक क्षण भी किसी को दुःख प्रिय नहीं है, दुःख से सारे चराचर को वैराग्य है-दुःख कोई नहीं चाहता आनंद को सभी ग्रहण करना चाहते हैं, उसका वैरागी कोई नहीं है-आनंद ब्रह्म-जो आनंद स्वरूप है, सर्व का प्रिय है भगवान, उनका जो ज्ञान उसे कहते हैं प्रिय संदेश।
प्रियः संदेशो यस्य सः प्रियसंदेशः प्रिय संदेश जिसका यानी भगवान आत्मा का अर्थात् भगवान आत्मा को सुनो। प्रियश्चासौ संदेशः प्रियसंदेशः - आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (इति श्रुतिः - भगवान आत्मा देखने योग्य है, सुनने, मनन करने एवं निदिध्यासितव्यः (इति श्रुतिः-भगवान आत्मा देखने योग्य है, सुनने, मनन करने एवं निदिध्यासन करने योग्य है। इसलिए हे गोपियों । तुम सब सुनो-प्रियश्चासौ संदेशः प्रियसंदेशः प्रिय ही जो संदेश और संदेश ही जो प्रिय ! अब यहाँ से सरकारी कलम शुरु होती है।
भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्वचित् ।
यथा भूतानि भूतेषु खं वाखग्निर्जलं मही ।।
(10-47-29)
तथाहं च मनः प्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयः ।।
(10-47-29)
मया सर्वात्मना भवतीनां वियोगः क्वचित् न मुझ सर्वात्मना भगवान से कभी किसी का वियोग नहीं है। अरे! मुझ परमात्मा से तुम गोपियों का कभी भी वियोग हुआ ही नहीं है। सुनो, यह तुम्हारा भ्रम है, मैं तो सर्व का सर्व, सर्व की आत्मा हूँ, सर्व का अधिष्ठान हूँ, सर्व का सर्व होने के नाते न मुझसे किसी का संयोग होता है और न वियोग। तुम लोग अपना कभी भी मुझसे वियोग न जानो-शरीर का संयोग, वियोग होता है, परन्तु सारे चराचर का जो अधिष्ठान है, जो चराचर का अस्तित्व है, उस आत्मा का न किसी से संयोग होता है न वियोग। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन पंच महाभूतों का किसी भी भूत से न संयोग होता है न वियोग। सारा चराचर पंच महाभूतों का ही तो कार्य है। डंडा भी पाँच भौतिक पदार्थ है, इससे पाँचों तत्व निकाल लो तो यह डंडा नहीं रहेगा। अर्थात् इस डंडे से पंच महाभूतों का कभी संयोग, वियोग नहीं है, क्योंकि यह डंडा पंच महाभूतों से भिन्न नहीं है। इसी तरह मुझ आत्मा का किसी से संयोग, वियोग नहीं होता। अरे ! पूर्ण का संयोग, वियोग कैसा? हाँ, शरीर का संयोग, वियोग होता रहता है।
भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्वचित् ।
यथा भूतानि भूतेषु खं वारविग्नर्जलं मही ।।
आत्मन्येवात्मनाऽऽत्मानं सृजे हन्म्यनुपालये ।
आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना ।।
(10-47-30)
आत्मना आत्मनि आत्मनं अहं सृजे, आत्मना आत्मनि आत्मानं अहं पालये, आत्मना आत्मनि आत्मानं अहं हन्मि । आत्मा करके आत्मा में आत्मा की मैं सृष्टि करता हूँ, आत्मा करके आत्मा में आत्मा का मैं पालन करता हूँ, आत्मा करके आत्मा में आत्मा का मैं संहार करता हूँ। तो फिर संयोग, वियोग कहाँ। यह अध्यात्म तत्व महाराज उद्धव गोपियों को सुना रहे हैं। 'मैं' करके 'मैं' में 'मैं' की सृष्टि, 'मैं' करके मैं में 'मैं' का पालन और 'मैं' करके 'मैं' में 'मैं' का संहार, तो फिर 'मैं' आत्मा में कहाँ संयोग और कहाँ वियोग-किसका संयोग कहें और किसका वियोग कहें। भगवान श्रीकृष्ण लिख तो मारे, अब समझो- आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजे हन्म्यनुपालये-'मैं' आत्मा करके 'मैं' आत्मा में 'मैं' आत्मा का सृजन, 'मैं' आत्मा करके 'मैं' आत्मा में 'मैं' आत्मा का पालन, 'मैं' आत्मा करके 'मैं' आत्मा का संहार क्या है? अरे! मैं जीव हूँ, यह सृष्टि किसने किया? 'मैं' आत्मा ने।
जीवं कल्पयते पूर्व ततो भावान्पृथग्विधान् ।
बाह्यानाध्यात्मिकां श्चैव यथाविद्यस्तथास्मृतिः ।।
(माण्डू.गौ.का.वैत.प्र. 16)
सर्वप्रथम अपनी आत्मा को आप ही जीव माना। किसने माना? मैं आत्मा ने। किस करके माना? मैं आत्मा करके। किसको माना? मैं आत्मा को माना। यही आत्मा करके आत्मा में आत्मा का सृजन होता है। जब तक यह मान्यता कायम है, बोध नहीं हुआ है, तब तक इस जीव सृष्टि का पालन हो रहा है। जब आत्मदेव का बोध हो गया तो जीव सृष्टि का संहार हो गया, ये बात। अरे भैया ! सुनो-सबसे प्रथम परमात्मा ने अपने आपको जीव माना। जीवं कल्पयते पूर्व-जीव की कल्पना की कि मैं संसारी जीव हूँ। यह गौड़पादीय कारिका है। इसके बाद अन्य भाव पैदा हुए। जीव विकल्प के बाद ही समस्त प्रपंच, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएँ, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय सब पैदा हो गये। यही 'मैं' करके 'मैं' में 'मैं' का पालन है और जब बोध हो गया, जब ज्ञान हो गया तो 'मैं' करके 'मैं' में 'मैं' का संहार हो गया।
आत्मन्येवात्मनाऽऽत्मानं सृजे हन्म्यनुपालये ।
आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना ।।
(श्रीमद् भा. 10-47-30)
अब प्रश्न हो रहा है कि परमात्मा ने अपने आपको जीव क्यों माना? जी हाँ-तो तुम्हारा इसमें क्या सिर दर्द है कि परमात्मा को क्या पड़ी थी, अपने आपको जीव मानने की, यही न? भैया! यह जो तुम्हारा प्रश्न है वह जीव देश का है कि आत्मदेश का? यह प्रश्न जीव देश का है। तो आत्मदेश में खड़े हो जाओ और फिर देखो, क्या ऐसा प्रश्न बनता है? उसने कभी भी अपने आपको क्या जीव माना है? आत्मदेश में तो ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता-तो फिर खतम- अरे! इसी का नाम तो संसार है। जब तक मान्यता कायम है तभी तक इसका पालन है और जब मान्यता गई तो संहार हो गया। गोपियों ! सुनो-जिस प्रकार महासागर में छोटी बड़ी लहरें उठा करती हैं और बड़े-बड़े ज्वार भाटे भी उठा करते हैं, और जिसमें ये छोटी-बड़ी लहरें उठा करती हैं ज्वार-भाटे उठा करते हैं सबके सब कालान्तर में उसी महासागर में समा जाते हैं। इसी प्रकार चैतन्याकाश महासागर में श्रीकृष्ण नाम की बड़ी भारी विभूति यानी ज्वार भाटा उठा है और श्रीकृष्ण के साथ ही राधिका, विशाखा, ललिता, किशोरी इत्यादि अनेक छोटी-बड़ी लहरें भी उठी हैं। समय पाकर ये सब के सब उसी चैतन्याकाश महासागर में समा जायेंगे। जो शेष रह जाएगा वही 'मैं' हूँ-भगवान आत्मा। तो फिर मुझ आत्मा में तुम्हारा संयोग वियोग कहाँ-मैं आत्मा श्रीकृष्ण में और मैं ही आत्मा तुम गोपियों में। इसलिए अब यह न मानो कि तुम्हारा और श्रीकृष्ण का संयोग, वियोग हुआ है। तुम लोगों की जो संयोग, वियोग की भावना है, यह सब तुम्हारे मन की बीमारी है। इसलिए मन का निरोध करो-मन को रोको, मन की लय कर दो। जब तक महाराज उद्धव ज्ञान की बातें बतला रहे थे, गोपियाँ चुपचाप शांति से सुन रही थीं, परन्तु जैसे ही मन का प्रसंग आया तो श्रीकृष्ण के प्रति जो उन सबकी आंतरिक भावना थी वह जाग उठी। कारण? ज्ञान देश में मन नाम की चीज नहीं है। वह योग का विषय है। जब महाराज उद्धव योग की बातें सुनाने लगे कि मन का निरोध करो तो फिर गोपियाँ मन देश में आ गई। गोपियाँ कहती हैं- हे महाभाग उद्धव ! अब बस ! बंद करो ! कृपा करो ! श्रीकृष्ण का संदेश सुनने के लिए अब हम लोगों के पास कान नहीं हैं। मन के निरोध की बातें अब बंद करो। श्रीकृष्ण कब से योगी हो गए? कब से वे ज्ञान की और योग की बातें करने लगे? क्या मथुरा जाते ही वे ज्ञानी और योगी बन गये। शायद कुब्जा ने सिखा दिया होगा। तो सुन लो यहाँ पर अब उनका योग न चलेगा। अपने श्रीमान् सखा से कृपापूर्वक कहियेगा कि इस योग को कुबरी के प्रति सुनायें, कुबरी मन का निरोध करे। अरे, भैया ! उद्धव, मन न भयो दस बीस -
उधौ मन भयो दस बीस ।।
एक रह्यौ सो गयो श्याम संग, को आराधै ईश ।
भई अति शिथिल सबै माधव बिनु, जथा देह बिनु सीस ।।
स्वाँसा अटकि रही आशा लगि, जीवहिं कोटि बरीस ।
तुम तो सखा श्यामसुंदर के, सकल योग के ईश ।।
सूरदास रसिकन की बतियाँ, पुरखौ मन जगदीश ।।
पाती में क्या लिखे हैं कि मन का निरोध करो-हे उद्धव ! किस मन का निरोध करें-एक मन रहा सो भगवान के साथ चला गया और एक ही मन सबके पास होता है, अब दूसरा मन कहाँ से लायें जिसका कि निरोध करें? अरे ! मन न भयो दस बीस-इसलिए हे उद्धव ! हमारे श्यामसुंदर उसी कुबरी को योग वैराग्य सिखायें। सारा दारोमदार तो कुबरी पर ही है। भैया! यहाँ से भी हम लोगों का संदेश लिख के ले जाओ-जाकर वहाँ पर, कुबरी को सुना देना-
वदन में बालकृष्ण, बेसर में पारब्रह्म,
चोटी में चक्रधर, अरु मोती में मुरारी है ।।
कर्णफूल में कमलापति, दामिनि में दीनानाथ,
हरवा में हरिजू, बाजूबंदन में गिरिधारी हैं ।।
सारी में साँवरो, किनारी में कन्हैया बसै,
अंगिया में अमरपति, अंग बसै बनवारी है ।
भौंहन में भगवान, कपोलन में कृपानिधान,
अंजन में मुरलीधर, और नैनन में बिहारी है ।।
और लिख के ले जाओ-
श्याम तन, श्याम मन, श्याम ही हमारो धन,
उधौ आठों याम हमें श्याम ही सों काम है।
श्याम हिये, श्याम प्रिये, श्याम बिनु नाहीं जिये,
अंधे की सी लाकड़ी अधार नाम श्याम है ।।
श्याम गति, श्याम मति, श्याम ही प्राण पति,
श्याम सुखदाई सो भलाई शोभाधाम है ।
उधो ! तुम भयो बौरे, पाती लै के आयौ दौरे,
योग कहाँ सीखूँ यहाँ रोम-रोम श्याम है ।।
गोपियों के मन का गुब्बार जब निकल गया तो कुछ शांत हुई और प्रेम से भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण कर महाराज उद्धव से पूछती है-हे उद्धव कहो, हमारे श्यामसुंदर आनंद से तो हैं न? मामा को मारकर अब तो वे राजा हो गये। क्या हम गाँव की ग्वालिनों की भी कभी सुधि लेते हैं? इस तरह प्रेम भरी चितवन से श्रीकृष्ण की लीला का स्मरण करती हैं। ब्रजबालाएँ महाराज उद्धव को उस सुखमय जीवन की, प्रभु की बाल लीला की झाँकी दिखाती हैं। जहाँ- जहाँ प्रभु ने लीलायें की थीं उन सभी जगह उद्धव को ले जाकर गोपियाँ दर्शन करतीं और प्रभु के प्रेमगान में विह्वल हो उठती हैं। उद्धव जी जब गोकुल आये तो सरकारी आज्ञा थी कि गोकुल में मेरा संदेश देकर जल्दी ही वापस आ जाना परन्तु उद्धव जी पूरे छः महीने तक नहीं लौट सके। जहाँ-जहाँ भगवान के क्रीड़ास्थल थे, सभी स्थानों में उद्धव गये और सब उद्धवजी का प्रेम से स्वागत करते रहे। महाराज उद्धव उनके प्रेम से सरोबार होकर ब्रजमंडल को धन्य जानकर प्रणाम करके रथ में बैठकर मथुरापुरी लौट आये।
- बोलो श्रीकृष्णचंद्र भगवान की जय -
श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव ।।
(कीर्तन)
षष्ठम दिवस
यदुवंशियों को ऋृषियों का शाप, भगवान कृष्ण का उद्वव को उपदेश हंसोपाख्यान
23-2-1969, प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
मंगलाचरण - नारयणोनिषत्
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्निबोधत । अनादिकालप से अविद्या के घोर अंधकार में सोने वालों भव्य जीवों! 'उत्तिष्ठत'- उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष के उपसन्न होकर अपना आत्म कल्याण करो-यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता के माध्यम से आत्मतत्व का निरूपण हो रहा है। कल के प्रसंग में आनंद-कन्द परमानंद भगवान श्रीकृष्ण की लीला पर प्रकाश डाला गया। बाल लीला से लेकर उद्धव-गोपी संवाद तक का प्रसंग बताया गया। जिस समय भगवान श्रीकृष्ण अपनी बाल लीला समाप्त कर, बकासुर, अघासुर आदि अनेक राक्षसों एवं कंस का वध कर चुके और महाभारत इत्यादि लीलाएं समाप्त हो गई तो किसी उसमय सप्तर्षियों का मंडल भगवान के दर्शन निमित्त द्वारिकापुरी को आया। मार्ग में यदुवंशी बालक, श्रीकृष्ण की पटरानी जाम्बवती के पुत्र साम्ब के पेट में एक लोहे की कड़ाही बांधकर उसे गर्भवती स्त्री का रूप बनाकर खेल रहे थे। जब सप्तर्षियों का मंडल उधर से निकला तो यदुवंशी बालक उन्हें घेर लिए और साम्ब को आगे करके पूछते हैं कि भगवन् ! इस स्त्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री? ऋषियों ने इसे बालकों का परिहास मानकर कहा कि तुम लोग अपना खेल खेलो, हमारा मार्ग मत रोको, हमें जाने दो। परन्तु यदुवंशी बालक बड़े दुराग्रही थे, वे न माने। फलस्वरुप ऋषियों ने शॉप दे दिया कि इसके गर्भ से न पुत्र होगा और न पुत्री बल्कि मूसल उत्पन्न होगा जिससे यदुवंशियों का संहार हो जायेगा। जब लोहे की कड़ाही को निकाला गया तो वह तत्काल मूसल हो गई। इससे बालक परम भयभीत हुए और द्वारिकापुरी आकर अपने से बड़ों को बताये, उन्हें भी दुःख हुआ और उस मूसल को यदुवंशी बालकों ने रगड़-रगड़कर लोहे का चूर्ण बना समुद्र में प्रवाहित कर दिया। जो छोटा-सा लोहे का अवशिष्ट भाग था उसे भी समुद्र में फेंक दिये। कालांतर में वह लोहे का चूर्ण बहकर प्रभास क्षेत्र में आ गया और चूर्ण का एक-एक कण सर्पत वृक्ष हो गया। जो छोटा-सा लोहे का टुकड़ा था उसको मछली निगल गई और जब मछुवे उस मछली को पकड़े तो लोहे का टुकड़ा निकला जो बाण का नोक बना। अभिशाप के कारण कुछ ही दिनों में द्वारिकापुरी में बड़े-बड़े असगुन होने लगे। तारे टूट-टूटकर गिरने लगे, पृथ्वी पर भूकंप आने लगा। श्रृंगाल असगुन बोलने लगे, दिन में उल्लू दिखाई देने लगे, नाना प्रकार का उत्पात होने लगा। इन अनिष्टों को देखकर भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर द्वारिकापुरी छोड़कर प्रभास क्षेत्र आ गये। द्वारिकापुरी में ब्राह्मण अभिशाप से उल्कापात हो रहा है तो प्रभास क्षेत्र चलकर यज्ञादिक कर्म करें ताकि शांति हो। यदुवंशीगण प्रभास क्षेत्र जाने के लिए तैयारी करने लगे तो उद्धव को भी इसका पता लगा। उद्धव जी शीघ्र ही आकर भगवान श्रीकृष्ण के श्रीचरणों में नतमस्तक हो प्रार्थना करते हैं-
देव देवेश पुण्यश्रवणकीर्तन ।
संहृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्ष्यते भवान् ।।
विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ।।
(श्रीमद् भागवत 11-6-42)
नाहं तवाङ्घिकमलं क्षणार्धमपि केशव ।
त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि ।।
(श्रीमद् भागवत 11 - 6 - 43
भगवन् ! मैंने सुना है कि यदुवंश के संहार के लिए ब्राह्मणों का अभिशाप हो गया है और आप अपनी योगलीला समाप्त करने वाले हैं। क्या आप ब्राह्मणों का अभिशाप मेटने में समर्थ नहीं हैं? और समर्थ होते हुए भी ब्राह्मणों का अभिशाप नहीं मेटना चाहते तो मुझे भी अपने साथ अपने धाम को ले चलिये, क्योंकि आपके चरण कमलों के आधे क्षण का भी वियोग सहन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ।
शय्यासनाटनस्थानक्रीडाशनादिषु ।
कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि ।।
(श्रीमद् भागवत 11-6-45)
सोने में, बैठने में, घूमने-फिरने में, खेल में एवं भोजनादिक सभी कार्यों में सदैव आपके साथ रहा। आप हमारे परम प्रिय हैं, आत्मा हैं। आपके वियोग में हम कैसे रह सकते हैं?
वातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः ।
ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ताः सन्यासिनोऽमलाः ।।
(श्रीमद् भागवत 11-6-47)
बहुत से ऐसे साधक हैं, जो वायु को रोककर प्राण और अपान वायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके ब्रह्म की उपासना करते हैं और अन्य, अन्य साधनों द्वारा संसार से तरने के लिए प्राण वायु को स्तंभित करते हैं। ऐसे कठिन कार्य कर ब्रह्मपद को प्राप्त करते हैं। परन्तु मैंने अपने आत्म कल्याण के लिए, संसार से तरने के लिए आज दिन तक कुछ भी साधन न किया।
वयं त्विह महायोगिन्भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु ।
त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः ।।
(श्रीमद् भागवत 11-6-48)
हे महायोगिन् ! मैं अनन्तकाल से कर्मों के जाल में पड़ा हुआ हूँ, कर्म कीचड़ से सना हुआ हूँ, मैं इस कर्मजाल से कैसे छुटकारा पाऊंगा? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। इतने दिनों से आपके सन्निकट रहकर भी मुझे कभी आत्मजिज्ञासा जागृत नहीं हुई। अब हे प्रभो! आप इस जगत से मुक्ति के उपाय का बोध करायें, क्योंकि आपकी यह माया बड़ी दुरत्यया है। इतनी भ्रामक एवं कठिन है कि इससे पार पाना अत्यन्त दुस्तर है। आपकी ही कृपा से इसे तर सकता हूँ। इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए। भगवान श्रीकृष्ण गोकुल से अक्रूर के साथ जब मथुरा आये तभी से उद्धव साथ में रहे। (सौ वर्ष मथुरा में रहे और पच्चीस वर्ष द्वारिकापुरी में, भगवान श्रीकृष्ण ग्यारह वर्ष वृन्दावन में रहे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक सौ पच्चीस वर्ष रहे) फिर भी उद्धव को आज दिन तक आत्म जिज्ञासा जागृत नहीं हुई। जब उद्धव को ही आत्मजिज्ञासा न जगी तो श्रीकृष्ण भगवान को क्या गरज पड़ी थी कि उद्धव को बोध कराते। जीव तो अपने संकल्प से ही बंधा है और अपने ही संकल्प से छूटेगा। गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।।
(गीता 6-5)
आत्म उद्धार अपने आप करता है, दूसरा कौन करेगा? जब वह स्वयं अपने आप अपने ही संकल्प से बंधा है तो दूसरा कौन छुड़ायेगा? हाँ गुरु, महात्मा संसारी जीवों को उपदेश करते हैं कि तू शरीर नहीं, आत्मा है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर से परे है। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था, भूत- भविष्यत्, वर्तमान तीनों काल में एकरस रहने के नाते तू आत्मा सत्य है। सर्व प्रपंचों का ज्ञाता है, इसलिए तू चेतन है। परम प्रेमास्पद होने के नाते तू आनंदस्वरूप है, तेरा कहीं आना-जाना नहीं। न मोक्ष, न बंध, न पाप, न पुण्य तू इन सबसे रहित परात्पर ब्रह्म आत्मा है। जिसको बोध हुआ उसका तो बेड़ा पार हो गया, नहीं तो आवागमन के चक्कर में लटका हुआ पड़ा है। आत्मस्वरूप को कोई भी जन्म जन्मांतर में न लख पायेगा जब तक कि उसको स्वयं ही आत्म जिज्ञासा न जागृत हो, अपने आपको जानने की भूख न लगे। वह भले ही विद्वान हो, परन्तु बोधवान न हो सकेगा। अब इतने दिन बाद उद्धव को आत्म जिज्ञासा जगी है। जिज्ञासुओं ! योगेश्वर भगवान अपना कर-कमलाङ्कित ज्ञान संदेश उद्धव के हाथ गोपियों के लिए भेजे थे और गोपियाँ भगवान के भेजे हुए ज्ञान संदेश को आदरपूर्वक सुनी, परन्तु उनको बोध नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? उनको बोध क्यों नहीं हुआ। जबकि ज्ञान संदेश स्वयं प्रभु ने अपने करकमलों द्वारा लिखकर अपने प्रिय सखा उद्धव द्वारा भेजा था?
न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ।
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्ह्यतर्व्यमणुप्रमाणात् ।।
(कठो. 1-2-8)
वेदों, शास्त्रों का चाहे कोई कितना भी प्रकाण्ड विद्वान क्यों न हो, परन्तु यदि उसे स्वस्वरूप भगवान आत्मा का बोध (साक्षात्कार) नहीं हुआ है तो उसके मुख से सुने हुए आत्म तत्व के उपदेश का विचार आत्म जिज्ञासु चाहे जीवन भर करता रहे, परन्तु उसे आत्म लाभ यानी अनुभव नहीं होगा। श्रोत्रिय तो है, परन्तु ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो ऐसे अज्ञानी गुरु के मुख से सुने हुए उपदेश से आत्मपद प्राप्त नहीं होता। विद्वान श्रुतियों, स्मृतियों के शब्दों का विश्लेषण करने में समर्थ हो सकता है। परन्तु, हाँ-यह निश्चय है कि उनके उपदेश से आत्म कल्याण न होगा। कारण? यह सिद्ध है कि एक पढ़ा-लिखा अज्ञानी और दूसरा अपढ़-अज्ञानी । अरे ! अज्ञानी तो दोनों ही हैं। अंधा अंधे को क्या बोध करायेगा। जब उसे स्वयं ही बोध नहीं हुआ है तो वह वस्तुतः अज्ञानी ही है, वह क्या दूसरे को बोध करायेगा। संसार में विद्वानों की कमी नहीं है, पहिले तो वेदांत के ग्रंथ संस्कृत में ही उपलब्ध थे, परन्तु अब सभी भाषाओं में हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली आदि में मिल रहे हैं। अब बाजार में सुगमता से खरीद लो। इससे वेदों के साहित्य का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा-साहित्य को पढ़ लोगे परन्तु बोध, यह बात दूसरी है-आत्मानुभूति दूसरी बात है। विद्वानों से प्रक्रिया, सिद्धांत भले ही पढ़ लो, परन्तु तुम्हें बोध न होगा। अब उद्धव गोपियों के गुरु हुए क्योंकि उन्होंने ही भगवान का कर-कमलाङ्कित ज्ञान संदेश गोपियों को सुनाया था। उद्धव, जिन्हें स्वयं आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, जो स्वयं बोधवान नहीं तो उनके द्वारा सुनाया गया यह विशुद्ध ज्ञान गोपियों तक कहाँ पहुँचे। जब गुरु ही ऐसे हैं तो फिर शिष्य का तो कहना ही क्या है।
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।।
(इति श्रुतिः मुण्ड, 1-2-12)
उस परम तत्व को जानने के लिए हाथ में पत्र, पुष्प लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो गुरु में दोनों बातें होनी चाहिए-प्रथम तो गुरु श्रोत्रिय यानी वेदों, शास्त्रों का प्रकाण्ड विद्वान हो और साथ ही ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे गुरु से ही शिष्य का कल्याण होता है। इनके ही आशीर्वाद से आत्मतत्व का बोध होता है। आत्मजिज्ञासु को ही स्वात्मानुभूति होती है। हाँ, ज्ञान के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं। इनको भी सुन लो- उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। जिस तरह भोजन के तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं-उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। भोजन का उत्तम अधिकारी वह है जिसे कस के भूख लगी है, दो दिनों से उसे भोजन नहीं मिला है और इसलिए इसका सिर चक्कर खा रहा है। उसे बड़ी भूख लगी है, बस, वह शीघ्रातिशीघ्र किसी तरह से क्षुधा निवृत्ति चाहता है। यदि उसे ऐसा कहा जाए कि भैया ! तुम तो ऐसे समय में आये कि चूल्हा-चौका उठ गया है, आप चाहें तो सेर सीधा ले लीजिए और स्वयं बना लीजिये, उसके लिए चूल्हा, कंडे, ईंधन सब मंगा देता हूँ, सभी इंतजाम किये देता हूँ, बना लो, तो वह उनके लिए राजी न होगा। उसे तो तीव्र भूख लगी है, रुखा-सूखा, ठंडा- बासी, कैसा भी भोजन हो, शीघ्र ही मिलना चाहिए। अब सुनिये, भोजन का मध्यम अधिकारी कौन है? मध्यम अधिकारी वही है जिसे अभी भूख तो नहीं लगी है, परन्तु बदहजमी भी नहीं है। ऐसे को यदि साधन बताया जाय तो वह राजी हो जाएगा। कारण कि अभी भी भूख नहीं लगी है। दो घंटे में जब तक भोजन बनेगा तब तक भूख भी लग जाएगी। तो वह भोजन के लिए साधन में जुट जाएगा। और भैया ! भोजन का कनिष्ठ अधिकारी कौन है? जिसके कंट तक लेटर-बॉक्स भरा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, बदहजमी है तो ऐसों को यदि षटरस छप्पन प्रकार का स्वादिष्ट भोजन भी ला दो तो भी उसका उसे क्या प्रयोजन है, वह क्या कहेगा-खीर ठीक नहीं है, इसमें तो चीनी कम है, हूँ कढ़ी खट्टी है, रोटी कच्ची ही रह गई है। वह सिर्फ तर्क करेगा, क्योंकि भूख तो उसको है ही नहीं। इसी तरह से ज्ञान के भी तीन अधिकारी होते हैं-उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम का आत्मानुभव में अधिकार होता है। मध्यम का साधन में अधिकार होता है। कनिष्ठ का शास्त्र में अधिकार होता है। उत्तम अधिकारी- जिसे आत्मजिज्ञासा और विषयों से तीव्र वैराग्य हो वह उत्तम अधिकारी है। जिसे जिज्ञासा तो है, परन्तु विषयों से वैराग्य नहीं वह मध्यम अधिकारी है। और जिसे न जिज्ञासा है, न वैराग्य है वह कनिष्ठ अधिकारी है। उत्तम अधिकारी आत्मानुभव चाहता है। मध्यम अधिकारी साधन चाहता है। कनिष्ठ अधिकारी शास्त्र प्रमाण चाहता है। उत्तम अधिकारी को कोई न कोई महापुरुष पहुँचकर आत्मतत्व का अनुभव करा देते हैं और मध्यम अधिकारी को साधन में लगा देते हैं। साधन दो प्रकार के होते हैं-एक पिपीलिका मार्ग और दूसरा विहंगम मार्ग। क्योंकि, अभी जिज्ञासु की जिज्ञासा मंद है, साधन द्वारा वह अपनी जिज्ञासा को तीव्र करे। अभी तड़प तो है नहीं इसलिए महात्मागण उसे साधन बताते हैं। पिपीलिका कहते हैं चींटी को, तो पिपीलिका मार्ग स्वामी वामदेव जी का है और विहंगम मार्ग महात्मा शुकदेव जी का है। जैसा जो अधिकारी होता है उसे उसी में महात्माजन लगा देते हैं। पिपीलिका मार्ग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और विहंगम मार्ग-श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि। कनिष्ठ अधिकारी को कुछ भी बताओ वह सोचेगा कि यह कहाँ लिखा है? इसका प्रमाण क्या है? जिज्ञासा तो है ही नहीं इसलिए वह तर्क करता है। उसकी बुद्धि तर्क में जाती है। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को महात्माजन शास्त्रों का थप्पड़ लगाते हैं। रामायण, गीता, भागवत पुराण, श्रुति, स्मृति आदि द्वारा उसकी बुद्धि को पराजित करते हैं इसलिए तीनों प्रकार के अधिकारी के कल्याण के लिए ब्रह्मनिष्ठ के साथ ही साथ श्रोत्रिय एवं साधन सम्पन्न होना जरूरी है। इसलिए जिज्ञासुओं को अपने आत्म कल्याण (लक्ष्य की प्राप्ति) के लिए किसी संत, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाना चाहिये।
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।।
इसलिए -
न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ।
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्ह्यतर्व्यमणुप्रमाणात् ।।
वेदों, शास्त्रों का प्रकाण्ड विद्वान हो परन्तु यदि वह आत्मानुभव से शून्य है, यदि उसे आत्म तत्व का अनुभव नहीं है तो ऐसे गुरु के उपदेश द्वारा बोध नहीं होगा। बोध तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु द्वारा सुनने से ही होगा। जीव का कल्याण तभी होगा। बिना बोध के आत्मतत्व का उपदेश करना ऐसा ही है जैसे कि-
अनुभूतिं बिना मूढो वृथा ब्रह्मणि मोदते ।
प्रतिबिम्बित शाखाग्र फलस्वादन मोदवत् ।।
(पंचदशी)
बिना अनुभूति के ब्रह्मज्ञान का उपदेश ऐसे ही है जैसे कि प्रतिबिम्बित फल का स्वाद बताना। किसी तालाब के किनारे आम का पेड़ है और फलों से लदा हुआ है। उसका प्रतिबिम्ब जल में पड़ रहा है। अब उस प्रतिबिम्बित फल का स्वाद बताना जैसा है, वैसा ही बोधशून्य गुरु का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना। जब फल ही पकड़ में न आया तो उसका स्वाद वह कैसे बतलायेगा? प्राप्त फल का स्वाद तो कोई भी बता सकता है, परन्तु प्रतिबिम्बित फल के स्वाद को कोई नहीं बता सकता। ऐसे गुरु के उपदेश द्वारा क्या लाभ होगा। हाँ- संसार में ऐसे उपदेशकों की कमी नहीं है। आजकल तो वेदांत हिन्दी आदि भाषा में प्रेस में छपते जा रहे हैं। पढ़कर ज्ञानी बन गये और दूसरों को उपदेश देने लगे।
कुशला ब्रह्मवार्तायांम वृत्तिहीनाः सुरागिणः ।
तेह्यज्ञानितमानूनं पुनरायान्ति यान्ति च ।।
(अपेरो.-133)
ब्रह्मवार्ता में तो कुशल हैं, परन्तु ब्रह्माकार वृत्ति से हीन हैं तो ऐसे लोगों का आवागमन कभी नहीं मिटता। गुरुघण्टाल वह जरूर बन सकता है, परन्तु अनुभव शून्य उपदेशक से आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बिना बोधवान गुरु के आत्मतत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो महाराज उद्धव और गोपियाँ दोनों को आत्म तत्व का बोध नहीं था। इसलिए भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कर-कमलाङ्कित होते हुए भी उस ज्ञान संदेश से गोपियों का आत्म कल्याण नहीं हुआ। वास्तविक विषय का बोध न उद्धव को था और न गोपियों को। दोनों एक ही कक्षा के विद्यार्थी थे। भगवान के आधिदैविक रूप की उपासिका गोपियाँ भी थीं और उद्धव भी थे।
उधौ तुम भयो बोरे पाती लैं कें आयो दौरे ।
योग कहाँ सीखूँ यहाँ रोम रोम श्याम है ।।
गोपियां सारा विश्व कृष्णमय देखती थीं। परन्तु मछली के समान भगवान के वियोग में तड़प रही थीं। कारण? भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध गोपियों को न था। अच्छा, अब अनुभव करो-भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? सुनो-देखो-नाम न लो-विकल्प मत करो-यह जो भास रहा है, यह भगवान का आधिभौतिक रूप है? यह क्या है? ऐसा विकल्प न करो-विकल्प करते ही यह जगत बन जायेगा और जो लीलाधारी रूप है वह भगवान का आधिदैविक रूप है-वह रज वीर्यात्मक नहीं है, संकल्पजन्य है।
इच्छामय नर वेश संवारे । होइहाँ प्रगट निकेत तुम्हारे ।।
(रा.बा.)
ब्राह्मण, संत, गौ, वेद की मर्यादा रखने के लिए, भगवान का यह आधिदैविक रूप प्रगट होता है। जो 'मैं' आत्मा हूँ वही भगवान का आध्यात्मिक रूप है। जो सर्व का सर्व है, जो सर्व में ओतप्रोत है। उद्धव और गोपियाँ दोनों भगवान के आधिदैविक स्वरूप के उपासक थे-दोनों का भगवान कृष्ण के प्रति सखाभाव था। देखो-4था अध्याय गीता का-
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ।।
(गीता 4-6)
मैं आत्मा अजन्मा, अविनाशी समस्त प्राणियों का ईश्वर यानी समस्त चराचर का शासक होते हुए भी (ईश्वर कहते हैं शासक को) अपनी प्रकृति के आश्रित होकर यानी अपनी माया करके जन्म धारण करता हूँ, अवतार लेता हूँ। यहाँ पर कौन कह रहा है? 'मैं' आध्यात्मिक स्वरूप भगवान आत्मा कह रहा हूँ। यहाँ पर आधिदैविक भगवान नहीं कह रहे हैं। कब जन्म धारण करता हूँ- अवतार लेता हूँ?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।
(गीता 4-7)
जब-जब धर्म की ग्लानि होती है अर्थात् धर्म का लोप होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब 'मैं' अपने आप की सृष्टि करता हूँ यानि अवतार लेता हूँ। किस प्रयोजन के लिए अवतार लेता हूँ? अवतार मुख्य तीन कार्यों के लिए लेता हूँ।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।।
(गीता 4-8)
भगवान का अवतार, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। आधिदैविक शरीर धारण करते हैं। यही तीन कार्य के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार के चार प्रकार होते हैं। नित्य, नैमित्तिक, आतुर और प्रादुर्भाव। भगवान के नित्य अवतार संत हैं और उनका कार्य धर्म की स्थापना है। नैमित्तिक अवतार- जब भी आवश्यकता हो उपरोक्त तीनों कार्यों के निमित्त होता है। राम, कृष्णादिक का अवतार रावण, कुम्भकर्ण, कंस, शिशुपाल, दन्तवक्र आदि दुष्टों का नाश, संतों की रक्षा और धर्म की स्थापना के निमित्त हुआ है। प्रादुर्भाव- भगवान का अवतार उसे कहते हैं जैसे भगवान का नृसिंहावतार हुआ है और आतुर अवतार है-हरि अवतार-गजेन्द्र मोक्ष के लिए। संत संसार में केवल एक ही काम करते हैं, धर्म की स्थापना। स्वरूप का बोध कराना, जन-जन में सार्वभौम सिद्धांत का प्रचार करना, विश्व के कोने-कोने में इस भागवत धर्म को फैलाना, यही उनका काम है। संत चाहे मार खा ले, परन्तु किसी को मारता नहीं है। संत का अवतार केवल एक ही काम करने के लिए है, जीव मात्र का कल्याण करना और संत स्वतंत्र होता है। अच्छा, तो यह जो लीला विग्रह स्वरूप, आधिदैविक अवतार है, इसे धारण किसने किया ? 'मैं' आत्मा ने। यदि 'मैं' को शरीर मानोगे तो यह परिच्छिन्न हो जाएगा और 'मैं' अपरिच्छिन्न हूँ। उस 'मैं' ने ही लीला विग्रह रूप धारण किया है, क्योंकि वस्तुतः ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त को धारण करने वाला 'मैं' ही हूँ। 'मैं' ने ही धारण किया है। यही भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है, यही उनका वास्तविक स्वरूप है। किसी समय सूर्यग्रहण का अवसर आया। भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकापुरी से रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि सभी पटरानियों सहित कुरुक्षेत्र पधारे कारण कि कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के अवसर पर स्नानादिक कर्म का महत्व है। उधर गोकुल वृन्दावन के ग्वाल बाल, गोपियाँ, महारानी राधिका जी, विशाखा, ललिता आदि ब्रजबालायें, बाबा नंद एवं यशोदा इत्यादि भी कुरुक्षेत्र आये थे। अब यहाँ पर जो संदेश उद्धव जी गोकुल में गोपियों को सुनाये थे और जिससे उन्हें बोध नहीं हुआ, वही ज्ञान संदेश जब भगवान के श्रीमुख से गोपियों को सुनने का अवसर मिला तो उनके हृदय की जो जीवग्रन्थि थी वह खुल गई और सबके सब उल्लास से कहने लगीं-कृष्णोऽहमस्मि-कृष्णोऽहमस्मि मैं कृष्ण आत्मा हूँ, मैं कृष्ण आत्मा हूँ। तब उन सबके चित्त को शांति मिली। श्रीकृष्ण भगवान का संदेश यही है कि 'मैं' सारे चराचर का अस्तित्व आत्मा हूँ और मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं।
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत ।
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ।।
क्योंकि भगवान आत्मा ही मूल है। इसके बिना जाने, बिना अनुभव किये, बिना सेवन किये, कभी भी किसी को चित्त में शांति न मिलेगी। इस चीज को धारण करने की जरूरत है। प्रभास क्षेत्र में जब महायोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण लीला समाप्त करने वाले थे तो उद्धव श्री चरणों के निकट बैठकर प्रार्थना करने लगे हे प्रभो, मेरा आत्म कल्याण कैसे हो? जिज्ञासा प्रगट कर रहे हैं। जीव का उद्धार चार कृपा से होता है-ईश्वर कृपा, सत् शास्त्र कृपा, आत्म कृपा और गुरु कृपा। हाँ-ईश्वर की कृपा यही है कि तुम्हें नर तन मिला-
कबहुंक करि करुणा नर देही। देत ईश बिनु हेतु सनेही ।।
ईश्वर कृपा तो हो चुकी। अब शास्त्र कृपा का स्वरूप सुनो-जितने सत् शास्त्र हैं, सत् शास्त्र उसे कहते हैं-जिस शास्त्र में किसी का खंडन न हो, सत्य वस्तु जो भगवान आत्मा है उसका ही प्रतिपादन हो। जैसे कि- श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण, उपनिषद सत् शास्त्र हैं। इन शास्त्रों में जिसमें भी तुम्हारी निष्ठा हो, आस्था हो, अटूट विश्वास हो उसे अपना इष्ट मानो। नित्य नियम से उसका पाठ करो, पढ़ो और चाहे एक ही श्लोक, मंत्र या चौपाई क्यों न पढ़ो परन्तु उस पर विचार करो, उसका मनन करो। खाली पाठ ही नहीं करना चाहिए। भाव को समझने का प्रयत्न करो। शास्त्रों को उपास्य कहते हैं। आराधक (उपासक) विचार करके उनके भावों को समझने की कोशिश करें। इस तरह से जब शास्त्रों की आराधना करोगे तो शास्त्र भगवान प्रसन्न होंगे। शास्त्रों की प्रसन्नता का लक्षण यही है कि शास्त्रों का गूढ़ से गूढ़ तत्व यानी छुपे हुए भाव तुम्हें लगने लगेंगे अर्थात् तुम्हारे हृदय में उन भावों का प्रकाश हो जायेगा, यही शास्त्र कृपा है। तीसरी कृपा आत्मा कृपा है। हृदय में आत्मजिज्ञासा का जागृत होना यानी 'मैं' अपने स्वरूप आत्मा को जानूं। इस प्रकार की प्रबल जिज्ञासा, मछली के समान तड़प जब पैदा होगी तभी आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने में अधिकार होगा और कोई न कोई संत की कृपा द्वारा बोध हो जाएगा। पहिले बता चुके हैं कि जिसको तीव्र भूख होगी वही भोजन का उत्तम अधिकारी है, वही भोजन के स्वाद की कदर करेगा। नाना प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया, शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त किया, शास्त्रों को पढ़ा, परन्तु पढ़कर भी यदि आत्म जिज्ञासा नहीं जागृत हुई तो सब पढ़ाई व्यर्थ है। कोई भी विद्यार्थी कॉलेज या स्कूल से आकर यदि उसका घर में रिह्वीजन नहीं करता तो उसे कुछ भी विद्या हासिल नहीं हो सकती। पास, फेल में क्या है जब तक आत्म जिज्ञासा तुममें बलवती नहीं है तो सद्गुरु मिल भी जाय तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते स्वाम् ।।
(मुण्डको. 3-2-3)
अयं आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः यह भगवान आत्मा जीवन पर्यन्त वेदांत का प्रवचन सुनने से नहीं मिलता। न बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। हृदय में जब तीव्र जिज्ञासा होती है अथवा आत्म दर्शन की तड़प होती है तभी भगवान आत्मा का अनुभव होता है।
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ।।
(मुण्ड. 3-2-4)
अयं आत्मा बलहीनेन न लभ्यः आत्मजिज्ञासा बल से हीन पुरुष को भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। न प्रमाद से, न तप से, न लिंग-अलिंग धारण करने से, इन उपायों से दर्शन नहीं होता। बल्कि आत्मानुभूति में आत्मजिज्ञासा ही परम साधन है।
यदि तुम्हारे हृदय में प्रबल आत्मजिज्ञासा है तो गुरु तुम्हारा नाम, गांव पूछते हुए तुम्हारे घर में स्वयं आकर तुम्हारा कल्याण कर जायेंगे। जिन संतों से आत्म दर्शन (तत्व का बोध) होता है उन गुरुओं का कोई खास भेश नहीं है। अवस्था, वर्ण, जाति नहीं है। न कोई खास जगह ही है जहाँ कि ऐसे गुरु की प्राप्ति हो सके। जिन्हें नारायण तत्व का बोध है वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। हाँ-तुम्हारे हृदय में श्रद्धा, विश्वास होना चाहिये। हमारे हृदय में गुरु के प्रति नारायण भाव होना जरूरी है। वह नारायण स्वरूप ही होता है। भैया! संसार सागर से तारने वाले नारायण ही होंगे। नर से क्या तरोगे जो कि स्वयं बोधवान नहीं है। कल्याण तो नारायण से ही होगा, नर से नहीं। नारायण ही नारायण को पायेगा जीव क्या नारायण तत्व का बोध प्राप्त करेगा। टेटकू-खचेडू जीव को भगवान कहाँ मिलेगा। परमात्मा स्वयंवेद्य है। यदि जीव को परमात्मा से भिन्न मानते हो तो परमात्मा चेतन है और चेतन परमात्मा से भिन्न जीव जड़ होगा। यदि जीव परमात्मा से भिन्न है तो सत्य परमात्मा से भिन्न जीव असत्य होगा, तो असत्य कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। यदि जीव परमात्मा से भिन्न है तो आनंद स्वरूप परमात्मा से भिन्न जीव दुःख रूप होगा, तो दुःख कैसे आनंद को प्राप्त कर सकता है। भगवान को भगवान ही जानेगा। भगवान को भगवान की प्राप्त करेगा। यह बड़ा विचित्र रहस्य है।
वयं त्विह महायोगिन्भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु ।
त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः ।।48।।
आत्मदर्शी महात्मा गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। सभी को सब समय नहीं मिलते। वेदांत का प्रवचन अनुभवी ही कर सकता है। यह साहित्य का विषय नहीं है। कितने गहरे पानी में पहुँचना पड़ता है, तब बोध कराया जाता है। हाँ-विद्वान बड़े-बड़े लच्छेदार भाषण वेदांत पर दे सकता है और उन प्रकाण्ड विद्वानों के भाषण सुनने में अच्छे लगते हैं। कर्ण प्रिय होते हैं, तुम्हारे मन में छाप बैठ जाती है कि प्रवचनकर्ता बहुत विद्वान है, बड़ा पंडित है, परन्तु विचारो तो मालूम होगा कि तुम्हें वस्तुतः कुछ नहीं मिला। गाँठ में क्या बांध लाये ? अनुभवी, बोधवान, विद्वान केन्द्र से बोलता है और केन्द्र तक ही पहुँचता है। अज्ञानी विद्वान कंठसे कहता है और तुम्हें कंठ तक ही पहुँचाता है। इसलिए बिना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के हर एक की सामर्थ्य नहीं है कि जो इस गोपनीय विषय को हृदय तक पहुँचा सके। हाँ जी! तो महाभाग उद्धव भगवान श्रीकृष्ण से जिज्ञासा प्रगट करते हैं-
वयं त्विह महायोगिन्भ्रमन्तः कर्मवर्मसु ।
त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः ।।
(11 - 7 - 48)
इसलिए महात्माओं से यही जिज्ञासा अभिव्यक्त करनी चाहिए कि भगवन् ! मेरा कल्याण कैसे हो? यदि तुम्हारी आत्म जिज्ञासा प्रबल है और मेरे प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें आत्म तत्व का बोध अवश्य होगा और यदि मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसका आत्म कल्याण नहीं होगा। मैं तुम्हें सावधान किये देता हूँ कि तुम कहीं मत भटको। दुनियाँ का भैया हमें बड़ा तजुर्बा है। भगवान के जिस नाम में श्रद्धा हो उस नाम का अखण्ड जप करो और भीतर से यह भावना करो कि हमारा आत्म कल्याण हो। भगवान के नाम का अखण्ड स्मरण कल्याणकारी है-मत भटको, हमारा कहना मानो, यही सीख है। हमने कोई मजहब, जमात, पंथ नहीं छोड़ा। सबका हमें अनुभव है, कही मत जाओ और यदि हमारे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास है, आये हो यहाँ, तो आत्म तत्व लख के जाओ, अनुभव करके जाओ। भैया ! संत नारायण होता है। वही तुम्हारा कल्याण करेगा जिसने स्वस्वरूप भगवान परम तत्व को प्राप्त किया है। आत्म कल्याण की भावना रख कर कीर्तन, ध्यान करो तो तुम्हें स्वयं तत्व का अनुभव हो जायेगा। परन्तु यदि आत्म कल्याण की भावना नहीं तो वहीं रुके रहोगे। जब तुम किसी स्टेशन पर जाते हो तो जो गाड़ी सामने होती है उसी में धमाके कूद नहीं पड़ते। पहिले पता लगाते हो कि यह गाड़ी कहाँ जायेगी? कहाँ-कहाँ रुकेगी? इसकी मंजिल कहाँ तक है और तब अपने गन्तव्य स्थान को जाते हो। यही बात अध्यात्म में भी है। साधक (मुसाफिर) को देखा देखी नहीं करनी चाहिए। संत, महात्मा, विद्वान साधन रूपी गाड़ी कहाँ से कहाँ तक पहुँचायेगी- पता लगा लो-नहीं तो सिद्ध बने घर में बैठो, कुछ नहीं मिलने का है। अभी तक कुछ नहीं मिला-अब करें, यह विकल्प मत करो। प्रथम आत्म कल्याण की भावना जागृत करो। फिर जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सके उसकी शरण में जाओ।
एवं विज्ञापितो राजन्भगवान्देवकीसुतः ।
एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुद्धवं समभाषत ।।
(श्रीमद् भागवत 11-6-50)
भगवान श्रीकृष्ण उद्धव की इस प्रबल आत्म कल्याण की जिज्ञासा को देखकर अपने अनन्य प्रेमी सखा उद्धव से कहते हैं-
यदात्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ।
ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वासं मेऽभिकाङ्क्षिणः ।।
(11-7-1)
भैया उद्धव । तुमको मैं यही कहता हूँ कि यद्यपि मैं ब्राह्मणों का अभिशाप मेटने में समर्थ हूँ, परन्तु जिसके लिए यह दिव्य लीला विग्रह स्वरूप मैंने धारण किया है वह सब कार्य पूर्ण हो चुका। देवताओं को अब कोई कष्ट नहीं रहा। उनका अभीष्ट कल्याण हुआ और दुष्टों का विनाश हो चुका। ब्रह्मादिक देवता अब आकर प्रार्थना कर गये कि प्रभो। सरकारी कार्य पूर्ण हो चुका है और अब लीला समाप्त हो। अब यदुवंशियों का आपस में लड़कर विनाश हो जाएगा कोई न बचेगा। हाँ, सुनो-यदुवंशी प्रभासक्षेत्र को जायेंगे और वहाँ ब्राह्मणों के अभिशाप के कारण उनका संहार हो जाने के बाद मैं भी अपनी लीला समाप्त कर दूँगा। उसी क्षण से कलियुग आ जाएगा। लीला समाप्ति के बाद, मेरे संकल्प से निर्मित जो द्वारिकापुरी है वह सातवें दिन समुद्र में डूब जायेगी, जलमग्न हो जायेगी। तुमको यही आदेश है तुम भी द्वारिकापुरी छोड़ देना।
मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः ।
यदर्थमवतीर्णोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ।।
(11-7-2)
त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु ।
मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग्विचरस्व गाम् ।।
(11 - 7 - 6)
स्वजन बन्धुषु स्नेहं परित्यज्य, सम्यक् प्रकारणे मनः मयि आत्मनि आवेश्य, समदृग्, भूत्वा, गाम् पृथ्वी विचरस्व। स्वजन परिवार के प्रति सर्वस्नेह (मोह) का परित्याग कर, मन को मुझ आत्मा में सम्यक् प्रकार से प्रवेश कर, समदर्शी होकर इस पृथ्वी मंडल पर विचरण करो, यही मेरी आज्ञा है। स्वजन का मतलब होता है-अपना बनाया हुआ, अपना माना हुआ, क्योंकि अपनी बनाई हुई चीज में ही स्नेह (मोह) होता है। स्वजन भाव, कुटुम्ब भाव तुम्हारा बनाया हुआ है। तुम ही बनाकर उसे संसार माने हुए हो। अब इस पर सुनो- अनुभव करो-सृष्टि दो प्रकार की होती है-एक जीव सृष्टि और दूसरी ईश्वर सृष्टि। इनमें भेद क्या है? हर एक की निगाह में (दृष्टि में) जो पदार्थ एक ही भाव से देखा जाय उसका नाम है ईश्वर सृष्टि । उदाहरण- अब दोनों लक्षण बतलाते हैं- जीव सृष्टि में भिन्न-भिन्न भाव जैसे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, पुण्यी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, परिछिन्न हूँ, जीने-मरने वाला हूँ, बद्ध हैं, मुक्त हूँ, अपने को कुछ का कुछ मान लेना, मैं-मेरा, तू-तेरा, यही जीव सृष्टि है और ईश्वर सृष्टि-इस मान्यता का जहाँ अभाव हो, वही ईश्वर सृष्टि है। देखो-अभी कोई शरीर यदि अपरिचित स्थान में चला जाय तो वहाँ के लोग सिर्फ यही मानेंगे कि यह मनुष्य है। और मनुष्य जाति में पुरुष है, तो यही ईश्वर जगत है। वही शरीर जब घर में आता है तो स्त्री उसे पति कहती है, पुत्र उसे पिता कहता है, माता उसे पुत्र कहती है, भाई उसे भाई कहता है। तो यह साढ़े तीन हाथ का मौजा मुश्तरकः है। परन्तु सभी अलग-अलग देख रहे हैं। यह शरीर कुछ बदला नहीं है, वही है परन्तु इस शरीर के कितने हिस्सेदार हैं, यदि स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब सभी अपना-अपना हिस्सा बँटवारा करें तो इस शरीर की हड्डी भी न बचेगी। पैर किसी को, तो सिर किसी को, कुछ न रहेगा यही जीव सृष्टि है। आत्म तत्व का बोध हो जाने पर जीव सृष्टि का अभाव हो जाता है। यह संसार नहीं है, जी, हाँ-सब वासुदेव है, सब नारायण है, इसमें जो विकल्प किया वही जीव सृष्टि है और बोध का फल है जीव सृष्टि का नाश। ईश्वर सृष्टि में किंचिन्मात्र भी दुःख नहीं है। इसलिये ज्ञान की जरूरत है। स्त्री का पति स्त्री के पास है, बहिन का भाई बहिन के पास है-जो जिसकी सृष्टि है वह उसी के पास है-यहाँ कुछ भी नहीं। कभी-कभी हमें निमंत्रण में ले जाते हैं और वहाँ पर अपने परिवार का फोटो हमें लाकर दिखाते हैं। कहते हैं-स्वामी जी ! यह मेरे पिता का फोटो है यदि वह ही है तो दुनियाँ में सभी को यह पिता दिखाई देता। तुम जो निगेटिव लेते यानि फोटो खींचते हो यह विकल्प का फोटो है या प्रतीति का? बिना डंडा उठाये नहीं बनेगा (पू. श्री स्वामी जी अपना डण्डा उठाकर कहते हैं) डण्डा है-लकड़ी पर डण्डे का विकल्प है, अच्छा-अब इसका फोटो लोगे तो प्रतीति का फोटो आयेगा कि विकल्प का? देखो कैसी पोल खुलती है यही संसार का हाल है। विकल्प तो तुम्हारे पास है-तुम उसे डंडा कहते हो- फोटो वस्तु (लकड़ी) का है न डंडा का। तुम्हारी पत्नी के लिए तुम पति भले हो, परन्तु शरीर में पति नहीं है। वह पति-पत्नी भाव मानने वाले के पास है। तो फोटो विकल्प का नहीं आता। यह तुम्हें पहले ही बताया जा चुका है कि-
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ।
(योग दर्शन)
शब्द तो सुनाई पड़े, परन्तु वस्तु का जहाँ अभाव हो उसे विकल्प कहते हैं। विकल्प का फोटो, निगेटिव नहीं होता। हाँ, उस प्रतीति का फोटो होता है। मेरी माता, मेरा पिता, मेरी घरवाली ऐसा कहते हो-बस, इसी का नाम संसार है, यही जीव सृष्टि है। प्रतीति को भगवान कहते हैं। यह ईश्वर सृष्टि है। इसलिए तुम अपने बनाये हुए संसार को त्याग दो-उसके मोह का त्याग कर दो-जीव सृष्टि दुःख रूप है। सुख-दुःख, पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म, जीना- मरना, यह सब जीव देश में है, ईश्वर देश में नहीं।
ईशावास्यमिद् सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ।।
(ईशा-1)
यह यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का पहला मंत्र है-जो कुछ भी यह स्थूल, सूक्ष्म है, सब ईश्वर है। जगती में जो कुछ जगत दिखाई दे रहा है-तेन त्येक्तेन उसका त्याग करके क्या करो? भुञ्जीथाः भोग करो। फिर कहते हैं- मा गृधः कस्यस्विद्धनम्-किसी के धन को ग्रहण मत करो-यहाँ पर धन का भाव धन नहीं है। अरे! धनम् का अर्थ हुआ अर्थम्। किसी के अर्थ को ग्रहण मत करो। जगत भाव को त्याग दो। चलो इसकी व्याख्या करें। यह जो सामने वासकिट पहने बैठा है, वह जगती (भास) है। अच्छा- अब इसमें नाम, रूप की कल्पना करो-बाबा बैठे हैं-यह जगत बन गया। अरे यार ! विकल्प ही तो जगत है। हाँ-यही जगती में जगत है। भास रहा है जगती और जहाँ कुछ माना नहीं कि वह जगत बन गया। जगत का व्याख्यान होता है, जगती का नहीं। तो किसी के अर्थ को ग्रहण मत करो। जैसा है वैसा ही रहने दो-अर्थ लगाना ही जगत है। यह अमुक वस्तु है, यही जगत है और इसी को जीव सृष्टि भी कहते हैं। अब तुम मानो या न मानो अमुक का फोटो नहीं आता। विकल्प ही तो इन्द्रजाल है।
सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला। जा पर होइ सो नट अनुकूला ।।
(रा.उ.का.)
दिल्ली में हमने किसी फोटोग्राफर से पूछा- भाई। यह तो बताओ तुम सरकारी प्रेस में हो, फोटो लेते रहते हो-जब जादूगर लड़की का सिर काट देता है और फिर जोड़ देता है तो क्या उसका फोटो तुमने कभी लिया है? तो उसने कहा स्वामीजी। हमने फोटो लेने का तो बहुतेरा प्रयत्न किया है, परन्तु फोटो नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? तो उसने कहा-हम इसे नहीं बता सकते। श्री स्वामीजी कहते हैं- भाई ! समझो, जब हो तब न आये। अरे! कुछ हुआ ही नहीं तो फोटो क्या आये। संसार सुन भर के कहते हो, परन्तु वस्तुतः इसके अंदर कुछ नहीं है, वस्तु शून्य है। तथ्य तो है ही नहीं। अपने स्वरूप के अनुभव (बोध) का यही फल है कि जीव जगत का सर्वदा के लिये नाश हो जाय। जगत में मेरा शत्रु-मित्र, भाई-बहन, पति-पत्नी, माँ-बाप नाना श्रृंखला लगी हुई है। परन्तु है कुछ नहीं। नाना विकल्पों का माया जाल बिछा हुआ है, नानात्व लगा हुआ है, यही संसार है। इसी का परित्याग करो-इसी का नाम भव सागर है। बिना बोध के जीव जगत का विनाश नहीं होता। बोध होने पर ही जगत का भ्रम का नाश होता है। जगत का भ्रम अकारण ही हो रहा है, है कुछ नहीं। जहाँ पर बोधवान जगती (भास) को नारायण आत्मा 'मैं' हूँ, ऐसा जानता है और अज्ञानी उस पर विकल्प करके जगत मानता है। इतना ही भेद है। बोध के बाद ही नारायण भाव होता है, वासनाओं का अंत होता है। 'मैं' आत्मा हूँ, यही ज्ञान है। हाँ-छोटे बच्चे घर-घरौंदा का खेल खेलते हैं। छत्तीसगढ़ में इसको घर-घुंदिया का खेल कहते हैं और यहाँ पर घर-घरौंदा कहते हैं। बच्चे घर के बाहर मैदान में किसी जगह बालू, मिट्टी आदि से घर बनाते हैं। कभी मिट्टी न मिली तो लकीर खींचकर घर बनाते हैं। बिल्डिंग तैयार करते हैं। नहाने, खाने, रसोई, सोने, बैठने आदि का कमरा बनाते हैं। मेहमान यहाँ ठहरेंगे-रसोई यहाँ बनेगी, यहाँ परछी (बराण्डा) आदि। है कुछ नहीं, परन्तु काल्पनिक मकान बना डालते हैं। वहाँ पर शादी-ब्याह भी करते हैं। पत्ते आदि की पूड़ी, कचौड़ी भी बनाते हैं और खाते भी हैं। परन्तु उससे उनकी भूख नहीं मिटती। हाँ भाई! पत्तों के काल्पनिक भोजन करने से क्या पेट भरेगा? बच्चे खूब मशगूल होकर खेलते हैं। उन्हें खेलते समय घर की याद नहीं रहती। यदि कोई उधर उनके काल्पनिक मकान से निकल जाये तो देखो कैसा हो-हल्ला मचाते हैं। बस, सर्वनाश हो गया समझकर रोते हैं। जब खेलते-खेलते ज्यादा समय हो जाता है तो फिर उन्हें भूख लगती है और तब उन्हें घर की याद आती है। फिर जिस मकान को इतनी मेहनत से हाथ से बनाये रहते हैं, उसे ही घर जाने के समय, पैरों से रौंद डालते हैं-घर को मिटा देते हैं। उसमें उनका तनिक भी मोह नहीं होता। ब्रजवासी बालकों से हमने एक शिक्षा ली है। जब ब्रजवासी बालक घर को बिगाड़ते हैं तो मंत्र कहते हैं-
मनुवा मर गयो, खेल बिगड़ गयो। मनुवा मर गयो खेल बिगड़ गयो ।।
यह बरसाने में हमने सुना है। तो हमने उनको गुरु बनाया। अरे ! मनुवा के रहते तक ही तो संसार रूपी खेल है और मनुवा मर गया तो खेल बिगड़ना ही है। स्त्री, पुत्र, शत्रु, मित्र, आलीशान मकान इत्यादि विकल्प रूप खेल बनाकर खेल रहा है और परमात्मा रूपी घर भूल गया है। बाद में जब याद आती है, जिज्ञासा पैदा होती है तब वह संत की शरण में जाता है। तब उसे भगवान आत्मा का बोध होता है। अनादिकाल का वैकल्पिक मकान जिसे वह स्वयं माना है-मन करके जो बना हुआ है, उसका नाश हो जाता है। भगवान उद्धव को उपदेश देते हैं कि इस विकल्प का अभाव कर दो।
त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु ।
भय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग्विचरस्व गाम् ।।
(11 - 7 - 6)
समदर्शी बनकर विचरण करो-समदर्शी का क्या मतलब है? सम अर्थात् सब में बराबर भाव। आत्म-जगत में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सब बराबर हैं, सम हैं, कोई ऊँचा-नीचा नहीं है। जो इस तरह से सभी में समभाव रखता है, कहीं भी भेदभाव नहीं है-
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।।
(गीता 6-30)
जो मुझ आत्मा को सब में देखता है और सबको मुझ आत्मा में देखता है, वह न मुझसे भिन्न है और न मैं उससे भिन्न हूँ। परन्तु हाँ-यह भाव बिना अपने स्वरूप आत्मा के बोध हुए नहीं आता। सभी शास्त्र, वेद, पुराण यही भाव व्यक्त करते हैं। इसी समदर्शी भाव को ग्रहण करके पृथ्वी पर विचरण करो। वेद, शास्त्र, संत, महात्मा-वैराग्यवान व्यक्ति को जब तक वह बोध प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने की आज्ञा नहीं देते। कारण कि जिन-जिन विषयों से उसे वैराग्य हुआ है उन्हीं विषयों का उसे दर्शन होगा। तो ऐसा न हो कि वह पुनः संसार में फँस जाय और उसका वैराग्य मंद पड़ जाये। यदि ऐसा हुआ तो जहाँ से वह चला था वहीं वापस आ जाएगा। कारण कि अभी समदर्शी नहीं हुआ है। आत्मबोध नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में यदि विचरण करेगा तो कहीं बंठाधार न हो जाय-यह आशंका लगी रहेगी। यदि विचरण करे भी तो स्वतंत्र रूप से नहीं, किसी संत, महान पुरुष की सेवा में रहकर उसके साथ विचरण करे। नहीं तो एकांत में गंगा के किनारे रहकर खुष्टन्याय के समान वैराग्य को पकावे और किसी संत की शरण में होकर बोध प्राप्त करे।
त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु ।
मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग् विचरस्व गाम् ।।
(11 - 7 - 6)
यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्थ्यां श्रवणादिभिः ।
नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम् ।।
(11 - 7 - 7)
भगवान उद्धव को कहते हैं- भैया! यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्याम् श्रवणादिभिः मन, वाणी, नेत्र, श्रवणेन्द्रिय एवं अन्य इन्द्रियों द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह सब नश्वर है। विषय ग्राह्य है और इन्द्रियाँ ग्राहक हैं। विषय पाँच हैं- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मन जहाँ तक मनन करे, बुद्धि जहाँ तक निश्चय करे, चित्त जहाँ तक चिंतन करे, वाणी जहाँ तक कथन करे, नेत्र जहाँ तक देखे, कान जहाँ तक सुने इत्यादि सबके सब नश्वर हैं, मनोमय यानी मनरचित है।
यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्थ्यां श्रवणादिभिः ।
नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम् ।।
(11-7-7)
अब यहाँ पर उद्धव का भगवान से प्रश्न होता है-भगवन्! किसी समय आप सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमारों को जो (हंस) रूप धारण करके तत्व का उपदेश दिये हैं, उस रूप और उस तत्व ज्ञान का मुझे उपदेश दीजिये वह प्रसंग मुझे समझाइए। उसे जानने की मेरी प्रबल इच्छा है-
यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव ।
योगमादिष्टवानेतदूपमिच्छामि वेदितुम् ।।
(11 - 13 - 15)
श्री भगवानुवाच -
पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः ।
पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकी गतिम् ।।
(11 - 13 - 16 )
हे उद्धव ! हिरण्यगर्भ जो भगवान ब्रह्माजी हैं उनके मानसिक पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमारों ने किसी समय अपने पिता ब्रह्माजी के पास जाकर सूक्ष्म जो योग की अंतिम गति है, उसे पूछा। अर्थात् आत्मानुभूति क्या है और उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये? इस पर भगवान कहते हैं-
यह श्रीमद् भागवत के एकादश स्कन्ध का 13 वाँ अध्याय है-
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो ।
कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरतितितीर्षोः ।।
(11-13-17)
गुणेष्वाविशते चेतो गुणश्येतसि च प्रभो-इन्द्रियों के जो विषय हैं, उन्हें गुण कहते हैं- हे प्रभो! शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पाँचों विषयों का चित्त में प्रवेश होता है अथवा इन विषयों में चित्त प्रवेश करता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु चित्त और विषय इन दोनों को अलग-अलग कैसे करें ? यह हंसोपाख्यान् है। मौलिक प्रश्न है- श्रीभगवानुवाच -
एवं पृष्ठो महादेवः स्वयंम्भूर्भूतभावनः ।
ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ।।
(11-13-18)
सनकादिकों के इस प्रकार पूछने पर स्वयंभू जो भगवान ब्रह्माजी हैं उन्होंने प्रश्नबीज यानी प्रश्नोत्तर देने के लिए ध्यान किया (कोशिश की) परन्तु प्रश्न जटिल होने के कारण उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए। कर्मजाल में फैसी हुई बुद्धि के कारण ब्रह्माजी इस आत्मपरक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्मकांडी की बुद्धि आत्मतत्व का विचार करने में समर्थ नहीं होती क्योंकि कर्मकांडी देहात्मवादी होता है। यह साढ़े तीन हाथ के शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर कर्म करता है। उसकी बुद्धि स्थूल होती है, क्योंकि यह निर्विवाद सिद्धांत है जो जैसा अपने आपको मानता है वैसी ही उसकी बुद्धि, उसके संकल्प एवं उसके कार्य भी होते हैं। इसलिए जितने भी कर्मकांडी हैं सब अध्यात्म से दूर रहते हैं।
उन्हें जूड़ी आ जाती है, भागते हैं। जब पितामह ब्रह्मा (विधाता सृष्टिकर्ता) की यह दशा है तो फिर संसारी कर्मकाण्डियों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार का प्रश्न जिज्ञासु राजा प्राचीनबर्हि ने भगवान नारद से किया था। उस दिन भी कहा गया था कि कर्मकाण्डी-देहात्मवादी होता है, उपासक-जीववादी और ज्ञानी-ब्रह्मवादी होता है। ॐशिव ! अध्यात्म में ये तीनों वाद छूट जाते हैं- न कर्म, न उपासना, न ज्ञान, कुछ नहीं रहता। ये तीनों बीमारियाँ यानी अध्यास साफ हो जाते हैं। भैया! यह बड़ा आरोग्य देश है।
शोक, मोह, भय, हरष, दिवस, निशि, देश, काल, जहं नाहीं ।
यही आत्मदेश का परिचय है-यह गोस्वामी जी की विनय पत्रिका है।
शोक, मोह, भय, हरष, दिवस, निशि, देश, काल, जहं नाहीं ।
तुलसिदास अस दशाहीन संशय निर्मूल न जाहीं ।। रघुपति भगति... ।।
हाँ-ऐसा सुंदर देश है कि कोई वादी नहीं। न कोई वादी है, न कोई प्रतिवादी। वकीलों को देखकर याद आ गई, भाई। यह विकल्प उठा। ऐसा सुंदर देश है-कर्मकाण्डी अपने को साढ़े तीन हाथ का देह मानता है। देह न मानेगा तो कर्म किससे करेगा, कैसे करेगा? इसी बुद्धि के कारण तो ब्रह्मा जी चकवर में पड़ गये, उनका मन खिन्न हो गया और इधर सनकादिकों को अभिमान हो गया। ब्रह्माजी के चारों मुख से चारों वेद-ऋग्, यजुः, साम, अथर्व निकले हैं। परन्तु कर्मासक्त होने के कारण ब्रह्माजी सनतकुमारों के प्रश्न का समाधान न कर सके। तो उनका चित्त विभुब्ध हो गया एवं लज्जित हो गये और उधर सनकादिकों को अभिमान हो गया कि हमारे पिता ब्रह्माजी भी हमार प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके।
एवं पृष्टो महादेवः स्वयंम्भूर्भूतभावनः ।
ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ।।
(11 - 13 - 18)
स मामचिन्तयद्देवः प्रश्नपारतितीर्षया ।
तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा ।।
(11 - 13 - 19)
उस समय जब ब्रह्मा जी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने मुझ भगवान आत्मा का चिंतन किया। भगवान का चिंतन क्या है? क्या चिंतन किया? देखो जीवन में जब कभी गंभीर प्रश्न या कोई जटिल समस्या आ जाती है, उसका समाधान नहीं होता कि क्या उत्तर देना है तो तुम निःसंकल्प हो जाते हो। यह निःसंकल्प होना ही भगवान आत्मा का चिंतन है। रात-दिन यार! सब के सब इसी में रहते हो, सारा प्रपंच करते हो, गंभीरता से सोचते हो। जहाँ मन को समेटकर निःसंकल्प स्थिति में स्थित हुए कि फट से उत्तर निकल आता है यही भगवान आत्मा का चिंतन है, स्मरण है। सभी रात-दिन इसी स्थिति में अपना व्यवहार पालन करते हैं। उस समय चित्त को निःसंकल्प करने के लिए कौन-सा साधन (अभ्यास) करते हो? जहाँ जब इच्छा हुई मन को निःसंकल्प कर लेते हो। कारण? चित्त पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। इतना आधिपत्य है कि जिस समय चाहो उसी समय निःसंकल्प कर लेते हो। मा ब्रूहिं दीनं वचः। शास्त्रों का यही उपदेश है। किसी से दिन वचन न बोलो। इस गरीबी को, हृदय को सुद्रता को निकाल दो। जब चाहते हो घंटों निःसंकल्प रहते हो, किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ-वैसे तुम निःसंकल्प होने के लिए साधन जगत में दौड़ लगाओ पर मिलेगा कुछ नहीं-यही मस्ती है। अरे। जहाँ बैठे हो, वहीं हम बता रहे हैं। तुम्हें उठाकर कहीं अन्यत्र नहीं सरका रहे हैं। यही प्राप्ति की प्राप्ति है। सब मस्त हैं। चाहे कोई विद्वान हो या अपढ़ हो, इसी मस्ती में सारा संसार मस्त है।
जो बतलावै साधना आप अधूरा होय ।
मिलत मिलावै राम सों सतगुरु कहिये सोय ।।
कोई नई चीज नहीं बतला रहे हैं-भैया। तुम अपने ही घर में हो, घंटों निःसंकल्प रहते हो। किताब पढ़ रहे हो-कानून पढ़ रहे हो, किसी विचार में मग्न हो, तो कितना निःसंकल्प रहते हो, अगर चित्त पर तुम्हारा आधिपत्य न हो, कमाण्ड न हो तो कैसे यह हो सकता है। यारों! सिर्फ इसको समझने की जरूरत है-इन्द्रियों पर, चित्त पर तुम्हारा पूर्ण आधिपत्य है।
यद्भायात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् ।
वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति यभयात् ।।
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ।।
(कठोपनिषद्)
जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से वायु बहती है, जिसके भय से इन्द्र वर्षा करता है, जिसके भय से अग्नि काष्ठ को दहन करती है। जिसके भय से मृत्यु चराचर को ग्रसता है, वह आत्मा 'मैं' हूँ। मेरा शासन तो सारे विश्व में है। 'मैं' अपनी हस्ती खींच लूं तो सूर्य भी नहीं रहेगा। यही मुझ भगवान आत्मा की महानता है। जी हाँ! हर वक्त तुम निःसंकोच हो, बस इसे ही समझना है। वैसे तो निःसंकोच अवस्था में ही बिना प्रयास के स्वभावतः समस्त व्यवहार रात-दिन हो रहे हैं। बिना किसी साधन के निः संकल्पता सिद्ध है। यदि साधन के द्वारा निःसंकल्पता सिद्ध करना चाहो तो यह संभव नहीं है कारण कि साधन का फल सदैव अनित्य होता है, नित्य नहीं होता। क्षणिक ही होगा, चिर (स्थाई) नहीं। जब तक साधन करते रहोगे तभी तक निःसंकल्पता रहेगी। जब तक साधन जगत में रहते हो तभी तक निःसंकल्पता भासित होती है, परन्तु जहाँ बाहर आये तो फिर मन संकल्प-विकल्प करने लगता है। इस अपनी महिमा को प्यारे ! भूलना नहीं। अपनी महिमा को न जानकर ही तुम साधन की अपेक्षा रखते हो। साधन द्वारा चित्त को निःसंकल्प करना ही अपनी महिमा का भूलना है। निःसंकल्प तो हो ही। विषयों की अनुभूति निःसंकल्प होकर ही करते हो। अभी यहाँ कथा सुन रहे हो तो निःसंकल्प अवस्था में सुन रहे हो या संकल्प-विकल्प की अवस्था में? निःसंकल्प अवस्था में। सारा विश्व निःसंकल्प है। इस महिमा से जिस समय अलग होता है, इस भगवत् महिमा से जब अलग होकर विकल्प करता है, ऐसी कल्पना करता है कि चित्त को साधन द्वारा निःसंकल्प करना है, तब फिर प्राणायाम, समाधि का अभ्यास करता है। परन्तु बार-बार साधन करता है और फिर भी साधन द्वारा क्षणिक निःसंकल्पता ही हाथ लगती है। इसलिए मुक्ता बार-बार यही कहता है कि भैया ! इसके लिए कुछ नहीं करना। कुछ किया नहीं कि बंठाधार हो गया, कुछ मिलने का नहीं। यह करने की चीज नहीं है, क्योंकि जो चीज कुछ साधन करके प्राप्त की जाती है, उसका कालांतर में नाश हो जाता है, क्योंकि साधन का फल अनित्य होता है। जो स्वयं सिद्ध है, वह साधन से क्या प्राप्त होगा? बस ! यह असाध्य रोग है।
तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा जी से सनकादिकों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझ भगवान आत्मा का ध्यान किया वह इसी निःसंकल्प स्थिति का पर्याय है। अरे यार! मुझ भगवान आत्मा के ध्यान में संकल्प- विकल्प कहाँ-तभी तो भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि- तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। सर्वकाल में मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। कन्हैया जैसा टेढ़ा है, वैसा ही उसका वचन भी टेढ़ा है। युद्ध भी कर और स्मरण भी कर। युद्ध सरीखे भीषण समय में अपनी रक्षा करना, सारथी की रक्षा करना, घोड़ों की रक्षा करना, और सन्मुख शत्रु को मारना इत्यादि कितनी भारी जिम्मेदारी सैनिक पर होती है और भगवान कहते हैं कि युद्ध कर और स्मरण भी कर। तो वह कौन-सा स्मरण है, जिसमें कि युद्ध भी होता रहे और स्मरण भी? यदि चित्त में संकल्प-विकल्प होता रहे तो फिर युद्ध और स्मरण दोनों नहीं होगा। इसलिए निःसंकल्प अवस्था में ही युद्ध और स्मरण दोनों कार्य हो सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने मुझ आत्मा का ध्यान किया तो मैं हंस रूप में प्रगट हो गया।
षष्ठम दिवस : दूसरी बेला
दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक
दृष्ट्वा मां च उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम् ।
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ।।
(11-13-20)
भगवान कहते हैं कि जब मैं हंस रूप में प्रगट हुआ तो मुझे वहाँ देखकर सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्माजी को आगे करके पादाभिवन्दनम् कृत्वा-मेरे चरणों की वंदना कर मुझसे पूछा कि को भवान्-आप कौन हैं?
इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्वजिज्ञासुभिस्तदा ।
यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे ।।
(11 - 13 - 21)
हे उद्धव ! तत्वजिज्ञासु सनकादिक ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर मेरे द्वारा जो कथन हुआ उसे तुम समझो। हालांकि उनका प्रश्न युक्तिसंगत यानी ठीक नहीं था, परन्तु थे तो आत्मतत्व के जिज्ञासु ही इसलिए उन्हें आत्मतत्व का जिज्ञासु जानकर आत्मोपदेश का अधिकारी समझकर मैंने उनसे कहा कि-
वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्न ईदृशः ।
कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मे क आश्रयः ।।
(11 - 13 - 22)
पंञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः ।
को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः ।।
(11 - 13 - 23)
सनकादिकों ! तुम लोगों ने जो पूछा है कि को भवान् - आप कौन हैं? तो किस दृष्टि को लेकर पूछा है? यदि आत्म दृष्टि से पूछा है तो आत्मा तो नाना नहीं है, अनाना है यानि एक है और जब आत्मा एक है तो जो आत्मा तुम हो वही आत्मा मैं हूँ-तो भला बताओ, एक में भी कहीं प्रश्न बनता है?
पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः ।
को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः ।।
(11 - 13 - 23)
और यदि शरीर दृष्टि से प्रश्न करते हो कि आप कौन हैं? तो शरीर भी पंच भूतात्मक होने के कारण एक ही है, वह अनेक नहीं है, जिन पंच तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है उन्हीं पंच तत्वों से ही यह हंस शरीर भी बना है और सारा चराचर ही पंच भूतात्मक है। इसलिए शरीर भी एक ही है। शरीर दृष्टि से भी तुम्हारा प्रश्न अनर्थ है, वाणी का विकार मात्र है। कहने का मतलब यह कि तुम्हारा प्रश्न न आत्म दृष्टि से बनता है और न शरीर दृष्टि से? यदि कोई शरीर पांच तत्वों से बना हो और कोई चार, छह तत्वों से बना हो तब तो शरीर अनेक कहा जा सकता है, परन्तु ऐसा नहीं है। इसलिए तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। सनादिकों की अभिमान हो गया था कि हमारे प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी भी नहीं दे सके तो भगवान ने पहले ही उनके अभिमान को नष्ट कर दिया, क्योंकि उनका प्रश्न ही गलत था। न तो आत्म दृष्टि से प्रश्न बनता है और न देह दृष्टि से। यदि अपने आपको आत्मा जानते हो तो आत्मा एक है, दो नहीं। इसलिए प्रश्न नहीं बनता और यदि अपने आपको शरीर मानते हो तो शरीर भी पंचात्मक होने से एक है, वह भी दो नहीं। इसलिए शरीर दृष्टि से भी प्रश्न नहीं बनता। इस तरह हंस भगवान सनकादिकों को उपदेश कर रहे हैं-
मनसा वचसा दृष्टया गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः ।
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ।।
(11-13-24)
मनसा वचसा दृष्टया मन द्वारा, दृष्टि द्वारा एवं अन्य इन्द्रियों के द्वारा भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब 'मैं' ही हूँ-मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं-इसको हे ऋषियों ! सरलतापूर्वक समझ लो-इसका अनुभव करो। आत्म जिज्ञासुओं ! इसको अच्छी तरह समझ लो-देखो उस समय के प्रसंग में भगवान श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा था-
यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्थ्यां श्रवणादिभिः ।
नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम् ।।
(11-7-7)
मन द्वारा, वाणी द्वारा एवं अन्य इन्द्रियों द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वह नश्वर है और अभी क्या कहते हैं- जो कुछ भी इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है वह सब 'मैं' ही हूँ। श्रीकृष्ण मुख से कहते हैं कि ये सब नश्वर है और अब हंस मुख से कहते हैं कि ये सब 'मैं' ही हूँ-तो अब समझो अब लगाओ इसका भाव तो भैया ! इन्द्रियों के ग्रहण काल में ये सब गुण यानी विषय नश्वर है और जिसका 'मैं' आत्मा अनुभव करता हूँ-वह 'मैं' ही हूँ। इसका भी अनुभव करायेंगे-तब पता चलेगा। देखो, इन्द्रियाँ जो हैं वह विषय को ग्रहण करती हैं कि वस्तु को ग्रहण करती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पाँचों विषय हैं। अच्छा, तो इन्द्रियों के ग्राह्य यही पाँचों विषय हैं। प्रश्न पहिले समझ लो-इन्द्रियों का ग्राह्य वस्तु है अथवा विषय? वस्तु से समझना आत्मा-तो सहज में समझ लोगे कि इन्द्रियों का ग्राह्य विषय है, वस्तु नहीं और विषय जो है वह विकल्प है, न कि वस्तु। विषय जो है वह विकल्प है अथवा विकल्पाधार? विषय विकल्प है। जितने शब्दादिक विषय हैं ये सब विकल्प रूप हैं और विकल्प अस्तित्वहीन होता है। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः (यो.द.)- शब्द का तो ज्ञान हो, परन्तु वस्तु का अभाव हो उसे विकल्प कहते हैं। तो सबसे पहले ग्राह्य का विकल्प होता है। ग्राह्य-विषय है और ग्राहक-इन्द्रियाँ। (ताली पीटकर स्वामी जी बता रहे हैं) यह शब्द विषय है। अच्छा-शब्द हुआ, परन्तु अभी इसका विकल्प मत करो। जब तक शब्द विषय का विकल्प न करोगे तब तक इसके सुनने के लिए कर्णेन्द्रिय नहीं पैदा होगी। ग्राहक और ग्राह्य दोनों का विकल्प एक ही काल में होता है। विषय और इन्द्रियाँ साथ- साथ ही बनती हैं। दोनों एक ही समय प्रगट होते हैं और इस व्यापार में मुझ आत्मा का क्या काम होता है? इन्द्रियाँ विषय को ग्रहण करती हैं और मैं आत्मा इसका अनुभव करता हूँ। अरे भाई! देखो कान से सुनाई पड़ा और कान से सुनाई नहीं पड़ा, यानी कान के सुनने और न सुनने का जो अनुभव करता है वह 'मैं' आत्मा हूँ। आँख के देखने को और आँख के न देखने को 'मैं' आत्मा अनुभव करता हूँ। इन्द्रियों का काम विषय को ग्रहण करने का है। विषयों के अनुभवकाल में यदि विषयानुभूति हो तब तो विषय है और यदि विषयों के अनुभवकाल में विषयानुभूति न हो तो 'मैं' ही हूँ। एक बार फिर अनुभव करायेंगे-विषय के अनुभवकाल में विषय का अनुभव न हो तो वह विषय नहीं है, 'मैं' ही हूँ। देखो-देख रहे हो? यह रूप विषय है-जिस समय द्रष्टा दृश्य को देखता है तो दृश्य के दर्शनकाल में द्रष्टा को (आगे-पीछे नहीं, बिल्कुल ठीक देखने के टाइम में) यह दृश्य है और मैं इसका द्रष्टा हूँ, ऐसा अनुभव होता है? नहीं। दृश्य के अनुभवकाल की अनुभूति हो, तब तो दृश्य है और नहीं तो दृश्य नहीं 'मैं' ही हूँ। द्रष्टा जब दृश्य का अनुभव करता है तो यही होकर अनुभव करता है या उससे भिन्न होकर यह इसकी समझने की दूसरी युक्ति है) वही होकर अनुभव करता है। बिल्कुल ठीक-वही होकर उसका अनुभव करता है। विषय बड़ा सूक्ष्म है-अरे भाई! यह मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि विषय ग्राह्य है और इन्द्रियाँ ग्राहक। विकल्प भाव में विषय है कि विकल्पाभाव में? विकल्प भाव में विषय है और ठीक अनुभवकाल में विकल्पाभाव है, तो वह 'मैं' ही हूँ। विकल्प भाव- यह ग्राह्य और इन्द्रियाँ-ग्राहक हैं। दोनों का विकल्प एक ही समय में होता है। लकड़ी न हो तो डंडा कहाँ, डंडे का विकल्प तो लकड़ी पर ही है। विकल्प रूप डंडे की स्वतंत्र सत्ता कहाँ-लकड़ी नहीं तो डण्डे का विकल्प भी नहीं। समस्त विकल्पों का आधार 'मैं' आत्मा हूँ। यदि 'मैं' आत्मा न होऊँ तो उन विकल्पों का आधार कौन होगा? इसलिए अहमेव - 'मैं' ही हूँ। इसको हे उद्धव ! तुम सरलतापूर्वक समझ लो। किसी विषय के अनुभवकाल में विषय है, ऐसा अनुभव नहीं होता। अनुभवकाल में विषय है ऐसा अनुभव हो तो विषय है, नहीं तो 'मैं' ही हूँ। 'विषयानुभूति ही स्वात्मानुभुति है'-इस सूत्र पर अब कुछ कहेंगे। जो दिखता है, वह दिखता है, 'मैं' दिखता हूँ, तब दिखता है, इस रहस्य को जान लिया फिर दिखना कहाँ जो दिखता है, देखने वाला ही है जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, वह दिख रहा है। क्या डंडा दिख रहा है? अरे! नहीं, लकड़ी दिख रही है। डंडा यदि लकड़ी के बिना दिखे तो डंडे का अस्तित्व है, नहीं तो लकड़ी ही है जो दिख रही है। 'मैं' के बिना यदि ये पाँचों विषय दिखे तब तो फिर इनका अस्तित्व है और बिना 'मैं' आत्मा के यदि ये नहीं दिखते तो इसका कोई वजूद नहीं रहता। तो मैं ही हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं इसलिए अहमेव। यह बात है- शिव ! इसलिए विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है-
श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कन्ध का पहला श्लोक-
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्,
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा,
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ।।
(श्रीमद् भागवत 1-1-1)
यहाँ पर महषि वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन के कुछ सूत्रों को ही छंदबद्ध करके रख दिया। यहाँ लिखा है- अर्थेष्वभिज्ञः अर्थेषुकोऽर्थः विषयेषु, अभिसम्यक् जानाति यः सः अर्थेष्वभिज्ञः । विषयों को जो सम्यक् प्रकार से जानता है उसे कहते हैं अर्थेष्वभिज्ञ। भगवान आत्मा जिस विषय को जानता है तो वही होकर उस विषय को जानता है इसलिए उसे अर्थेष्वभिज्ञ कहते हैं। अब समझो यदि विषय से 'मैं' भिन्न हूँ तो विषय नहीं और अभिन्न हूँ, तो फिर अहमेव। इसी प्रकार मन को ले लो-जिस मन से सभी परेशान हैं-मन है-यह जो 'है' है वह मन का है या मैं आत्मा का ? 'मैं' आत्मा का है। तो फिर मन का अस्तित्व 'मैं' आत्मा हूँ कि मन? मन का अस्तित्व 'मैं' आत्मा हूँ। मन यदि 'मैं' से भिन्न है तो मन नहीं और अभिन्न है तो 'मैं' ही हूँ जिसका नाम मन है। लहर है-तो लहर का अस्तित्व जल है कि लहर? लहर का अस्तित्व जल है, क्योंकि जल के बिना लहर का अस्तित्व ही नहीं रहता। यदि लहर को पकड़ने चलो तो लहर को न पकड़ पाओगे। तो क्या पाओगे? जल। इसी तरह किसी भी देश, काल, वस्तु का कुछ भी अस्तित्व नहीं है इसलिए अहमेव। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। विकल्पों का जाल बिछा हुआ है।
मनसा वचसा दृष्टया गृह्ययेऽन्यैरपीन्द्रियैः ।
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ।।
(11-13-24)
अहमेव - 'मैं' ही हूँ। देखो-जिस तरह मुझ आत्मा के बिना मन नहीं इस तरह आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। इन्द्रियाँ किसे कहते हैं? पंच विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सत, रज, तम यह किसे कहते हैं? अपने 'मैं' को (अस्तित्व को) निकाल लो, यदि वह वस्तु रहे तब तो समझो कि वह है- परन्तु उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं तो फिर वह अहमेव - 'मैं' ही हूँ। मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। सत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं। अपने 'मैं' अपने स्वरूप आत्मा से किसी भी चीज को अलग करके देखो। यह डंडा है-यह इन्द्रियाँ ग्राह्य विषय है। विकल्प इन्द्रिय ग्राह्य है न कि प्रतीयमान। प्रतीति कहते हैं भास को-प्रतीति का अर्थ देखना नहीं होता, प्रतीति का अर्थ भासना होता है। महीने दो महीने का बच्चा है, उसके लिए यह सब संसार विषय केवल प्रतीति मात्र है। वह प्रतीयमान जगत में रहता है, विकल्प जगत में नहीं रहता। बालक के सामने यदि सिंह भी आ जाय तो भी उस बालक को कोई भय नहीं है, उसे भय न लगेगा, क्योंकि उसे सिंह भासता है और जो विकल्प करेगा कि सिंह है तो फिर वह डरेगा-उसके हाथ पैर ढीले पड़ जायेंगे। बालक के लिए सिंह विकल्पाभाव है और दूसरों के लिए विकल्पभाव है। विकल्प ही इन्द्रिय ग्राह्य है और जिस पर यह विकल्प है वह 'मैं' ही हूँ। यह जो कुछ प्रतीत हो रहा है, यह दिख नहीं रहा है, भास रहा है। विकल्प न करो कि यह डंडा है, जब विकल्प न करोगे तो दिखेगा कि भासेगा? भासेगा। (ताली पीटते हैं)- विकल्प न करो कि यह शब्द विषय है? भास है। तो इन्द्रिय ग्राह्य विकल्प है और भास है वह 'मैं' ही हूँ इसलिए अहमेव क्योंकि प्रतीति में भय नहीं-भय तो वैकल्पिक जगत में है, 'मैं' में कहाँ। जो प्रतीति है वह भगवान आत्मा 'मैं' हूँ। प्रतीति पर जो विकल्प है वह संसार है और यही इन्द्रिय ग्राह्य विषय है। सिर्फ विकल्प हटा देना है-वस्तु तो पहले से ही परिपूर्ण है इसलिए जो विकल्प है वह मनोमय है, नश्वर है। नश्वर और प्रतीति है, भास है, वह 'अहमेव'। भगवान का कहना यही है।
मनसा वचसा दृष्टया गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः ।
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ।।
(11 - 13 - 24)
देखो-इस गाँव को क्या कहते हैं? झंडापुर। तो भैया ! यहाँ इतने बैठे हो जरा कोई आकर हमें झंडापुर हाथ से पकड़कर दिखा दो कि यह झंडापुर है- क्या यह मकान झंडापुर है या यह सामने जो महुआ का पेड़ है वह झंडापुर है? सुनी सुनाई बात न बताना-ठीक-ठीक बताना-हमें हाथ से झंडापुर पकड़वा दो-तो भैया ! ढूँढ़ने चलोगे तो तुम्हें झंडापुर न मिलेगा-कारण? झंडापुर एक विकल्प है, न कि प्रतीति। इसी तरह न कुंडा तहसील, न उत्तर प्रदेश, न भारत वर्ष, न संसार। संसार भी नहीं 'अहमेव'- 'मैं' ही हूँ। भगवान कहते हैं कि इसको सफलतापूर्वक समझ लो-इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, यदि बुद्धि से समझने की कोशिश करोगे तो कठिनाई है, परन्तु 'मैं' को 'मैं' से समझने में कोई कठिनाई नहीं है। वाह 'मैं' ही 'मैं' को समझा रहा है। भगवान के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। इसलिए 'अहमेव'।
साकी ने वहदत का एक जाम पिलाया था।
उस रोज से हर कतरा दरिया नजर आता है ।।
वासुदेवः सर्वमिति-आत्मैवेद् सर्वंम्-सब 'मैं' ही हूँ। स एवेदं सर्वम्-
जिधर देखता हूँ जहाँ देखता हूँ ।
मैं अपनी ही ताव और शाँ देखता हूँ ।।
शमां का मैं हूँ परवाना, कोई कुछ समझै कोई कुछ समझै ।
यार पे मैं हूँ दीवाना, कोई कुछ समझै कोई कुछ समझै ।।1 ।।
यार की यारी में खोया, जितने दुनियाँ के थे फंदे ।
है यही यार का याराना, कोई कुछ समझै कोई कुछ समझै ।।2 ।।
वहदते पिलाया मय साकी, दिल जेर ज़बर बेलाम हुआ ।
वरहना घूमता मस्ताना, कोई कुछ समझै कोई कुछ समझै ।।3 ।।
वरहना कहते हैं नंगे को। जब तक यह मान्यता है कि मैं अमुक हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थी, वानप्रस्थी हूँ, संन्यासी हूँ, तब तक मान्यता जगत है और जब अहंभाव दूर हो गया-माया से परे हुआ, समस्त अमुक भावों (विकल्पों) का जब अभाव हो गया-मान्यता न रही कि मैं अमूक हूँ, तो रह गया वरहना। यही तो पर्दा था कि कुछ न कुछ अपने आपको मानना, मान्यताओं के आड़ में ही पर्दानशीं बैठा हुआ है।
वहदते पिलाया मय साक्री, दिल जेर ज़बर बेलाम हुआ ।
वरहना घूमता मस्ताना, कोई कुछ समझै कोई कुछ समझै ।।3।।
मस्ताना डोलत फिरै ज्यों सरकारी सांड़-सांड़ दो प्रकार के होते हैं-एक लोकल और दूसरा सरकारी। लोकल सांड़ को कभी-कभी कांजी हाउस में भी डाल देते हैं और कभी जोत भी लेते हैं-परन्तु सरकारी सांड़-उसके पुढे पर सरकारी मुहर लगी रहती है-कहीं जाय, कहीं सोये-कोई कहने वाला नहीं है।
मस्ताना डोलत फिरै, ज्यो सरकारी सांड़ ।
डर काहू की है नहीं, खसम बिना जस रांड़ ।।
अरे भाई खसम के रहते तक ही तो डर है।
खसम बिना जस रांड़, चाहै जागै चाहै सोवै ।
मन माना जग मुआ, भला अब किसको रोवै ।।
कहता मुक्ता सत्य, मान बिन जिसने जाना।
हुआ निरंकुश पुरुष दीवाना मस्ताना ।।
तो भैया !
बेचश्म हुआ तब चश्म खुली, बेजिस्म हुआ तब जिस्म मिली ।
कुछ रहा न अपना बेग़ाना, कोई कुछ समझै कोई कुछ समझै ।।4।।
जब तक साढ़े तीन हाथ की निगाह थी तभी तक मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर है, यह मान्यता थी, भगवान से दूर था और जब मान्यता चली गई अर्थात् बेचश्म (बिना आँख का) हो गया, सीमित दृष्टि खतम हो गई तो अंदर की आँख जो दिव्य दृष्टि है वह खुल गई। जब इस शरीर का भाव नहीं रहा, इसके अस्तित्व का अभाव हो गया, तब सारा चराचर अपना ही स्वरूप भासने लगा।
खुदी गुमी गुमशुदा मिला, तमन्नायें सब काफूर हुई ।
पस हो गई दुनियाँ अफ़साना, कोई कुछ समझै कोई कुछ समझै ।।5।।
जब खुदी अर्थात् देहाभिमान नष्ट हो गया तब गुमशुदा यानी जो खोया हुआ था, जिसके स्वरूप का अज्ञान था, पता नहीं था कि कहाँ है, वह सच्चिदानंद घनभूत परमात्मा प्राप्त हो गया। उसके स्वरूप का बोध हो गया। जब शरीर से भिन्न अपने 'मैं' को जाना, पहचाना तो तमन्नायें काफूर हो गईं। पस-इसलिए, अफसाना-कहानी, तमन्नाएं-आशाएं।
मुक्ता जब मिला समुंदर से, फिर कौन किसी को याद करै ।
बस इसी लहर में लहराना, कोई कुछ समझै कोई कुछ समझै ।।6।।
नदी जब समुद्र में मिलती है तो नदी को यह याद नहीं रहता कि आज के पहले मैं गंगा, यमुना थी, अब समुद्र हो गई। जब नदी को यह भान हो कि मैं अमुक हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, तो समझ लो कि अभी समुद्र से उसका मिलाप नहीं हुआ है। जब संत कृपा से, गुरु कृपा से, सेल्फ रियलाइजेशन (स्वरूप का ज्ञान) हो जाता है तो इसके पहिले मैं जीव था-अब ब्रह्म हुआ, मैं ब्रह्म हूँ, तुम जीव हो, ये सब भाव नहीं रहते। हाँ-जब तक ऐसा भाव है तो जान लो कि अभी कुछ नहीं पाया।
मुक्ता जब मिला समुंदर से, फिर कौन किसी की याद करै ।
बस इसी लहर में लहराना, कोई कुछ समझै कोई कुछ समझै ।।6।।
आज के पहिले 'मैं' ही था और आज भी 'मैं' ही हूँ और आगे भी 'मैं' ही रहूँगा। तो इसका क्या प्रमाण है कि आज के पहिले 'मैं' ही था? यदि कहो कि आज के पहिले 'मैं' नहीं होता तो पुनर्जन्म किसका होता? तो जाने दो- पुनर्जन्म तो जीव जगत की बात है। मीमांसा दर्शन तो जीव जगत के ही लिए है, भगवान आत्मा के लिए नहीं। इसलिए आज के पहिले 'मैं' ही था, इसका क्या प्रमाण है? अरे ! इसका प्रमाण 'मैं' ही हूँ, इसका प्रमाण मैं ही होऊँगा- कोई दूसरा थोड़े ही होगा-कैसे? यदि कहो कि आज के पहिले 'मैं' नहीं था तो 'मैं' के नहीं था को नहीं था ने देखा था कि था ने देखा? अरे ! 'मैं' के अभाव का साक्षी यानी 'मैं' नहीं था और 'मैं' नहीं था, इसको कौन जानता है? इसका अनुभवकर्ता कौन है? आज के पहिले भी 'मैं' था, इन दोनों को सिद्ध करने वाला तो 'मैं' ही हूँ। आगे भी 'मैं' ही रहूंगा और 'मैं' नहीं रहूंगा इसको भी सिद्ध करने वाला 'मैं' ही हूँ 'मैं' ही अनुभवकर्ता हूँ। सब का सिद्ध करने वाला 'मैं' ही हूँ। आत्मा कहते हैं अस्तित्व को। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सारे चराचर का विकल्प मुझ आत्मा पर ही है। वस्तु तो एक ही है, विकल्प अनेक करते रहो, चाहे जो मर्जी हो। विकल्प इन्द्रिय ग्राह्य है-विकल्पाभाव अहं ग्राह्य है-प्रतीति अहं ग्राह्य है। इस तरह जो इन्द्रिय ग्राह्य है वह नश्वर है और प्रतीति जो अहंग्राह्य है वह अहमेव-वह तो 'मैं' ही हूँ।
मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः ।
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ।।
(11 - 13 - 24)
इसको हे उद्धव ! तुम अच्छी तरह से सरलतापूर्वक समझ लो।
जब भगवान हंस रूप से सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषियों को प्रबोध कर चुके तब फिर जो प्रश्न इन ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्माजी से किया था उसे समझाने लगे।
गुणेष्वाविशिते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः ।
जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः ।।
(11-13-25)
सनकादिकों ! गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः तुम लोगों ने यह पूछा था कि विषयों में चित्त प्रवेश करता है कि विषय चित्त में प्रवेश करते हैं? तो सुनो-विषय और चित्त ये दोनों जीव के देह हैं-जीवस्य देह उभयं और वस्तुतः चित्त और विषय इन दोनों की मुझ आत्मा से ही उत्पत्ति जानों, क्योंकि 'मैं' आत्मा सर्वाधार हूँ। देखो सुषुप्ति अवस्था गाढ़ी नींद में जब चित्त नहीं रहता, अपने कारण अज्ञान में लीन हो जाता है तो मैं जीव हूँ, क्या यह भाव रहता है? चित्त के अभाव में जीव भाव नहीं रहता इसलिए चित्त जीव का देह है और विषय के बिना जीव का जीवन नहीं इसलिए विषय जीव का दूसरा देह है। गुणाश्चेतो मदात्मनः गुण और चित्त दोनों को मुझ आत्मा से जानो। दोनों का विकल्प किस पर हुआ? मुझ आत्मा पर तो इन दोनों का आधार 'मैं' आत्मा हूँ। इसलिए-
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः ।
जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः ।।
(11 - 13 - 25)
गुणेषु चाविशच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया ।
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत् ।।
(11 - 13 - 26)
यह जो चित्त है वह विषय का सेवन करते-करते विषय रूप ही हो जाता है। तो सनकादिकों, इन दोनों को एक-दूसरे से अलग करने की आवश्यकता नहीं है। मद्रूप उभयं त्यजेत-चित्त और विषय दोनों को अपना स्वरूप जानकर, अनुभव कर दोनों का परित्याग कर देना चाहिए। यहाँ गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए इसी विषय को समझाते हैं-
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।।
(गीता 6-34)
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।।
(गीता 6-35)
अभ्यास और वैराग्य से इसको पकड़ना चाहिए-यहाँ अभ्यास और वैराग्य का क्या स्वरूप है? अभ्यास नहीं करना, यही अभ्यास है और जगत का अस्तित्व तीनों काल में है ही नहीं, यह जानना वैराग्य है। बात तो है सही, सोलह आना-परन्तु है-अभ्यास न करना, यही अभ्यास है। आज दिन तक मन के मारने का, मन को न रोकने का अभ्यास किये हो, अब मुक्ता की वाणी पर विश्वास करके, मन को रोकने का, अभ्यास करके देखो-जो दवा फायदा करे उसी को खाओ। हाँ-एक बात हम कहेंगे, अपने आपको संसारी जीव मानकर नहीं, अपने आपको भगवान आत्मा जानकर करो। इतना तो संशोधन हम अवश्य करेंगे। भाई ! अपने आपको संसारी जीव मानकर ही तो तुम मन रोकने का अभ्यास करते हो और तुम्हें आज तक क्या मिला, इसके साक्षी तुम स्वयं हो। अब लो-अपने आपको शरीर से भिन्न आत्मा जानकर मन के न रोकने का अभ्यास करो। पुड़िया फायदा करे तो खाओ और नहीं तो मन के रोकने का अभ्यास तो कर ही रहे हो। मन को रोकने को रोकना यही तो अभ्यास है और मन तीन काल में है ही नहीं-यही त्याग है। इसी का नाम वैराग्य है। यहाँ देखो-घर में जाकर जो पुड़िया फायदा करे सेवन करो-हम तो लाखों को इस पुड़िया से फायदा पहुँचाये हैं, यह बड़ी हाई पोटैन्शी पुड़िया है। इसके सेवन करने से मर्ज और मरीज दोनों खतम हो जाते हैं। प्रश्न होता है कि स्वामी जी ! मर्ज तो जाना चाहिए, ठीक है परन्तु मरीज को क्यों खतम करते हो? भैया ! जब मर्ज ही न रहा तो मरीज किसको कहोगे-बस, अपने आपको जानकर, मानकर नहीं-जानकर, अब कुछ न करने का अभ्यास करो।
जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः ।
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ।।
(11-13-27)
जाग्रत स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, मन की ये तीनों अवस्थायें तीन गुण की हैं। रजोगुण की जाग्रत अवस्था, तमोगुण की सुषुप्ति अवस्था और सतोगुण की स्वप्नावस्था। परन्तु तासां विलक्षणो जीवः - जीव इन तीनों अवस्थाओं से विलक्षण है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं से परे और साक्षी है, ऐसा जानो।
जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः ।
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ।।
(11 - 13 - 27)
यर्हिसंसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः ।
मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्त्यागस्तद्गुणचेतसाम् ।।
(11-13-28)
ये बात - तीन गुण की जो तीन अवस्थाएँ हैं- जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, वही संसार है और आत्मा का बंधन है, तो फिर 'मैं' जो आत्मा तुरीय पद हूँ उसमें स्थित होकर गुण और चित्त दोनों का परित्याग कर दें।
अहंकारकृतं बन्धमात्मनोर्थविपर्ययम् ।
विद्वान्निर्विद्य संसारचिन्ता तुर्ये स्थितस्त्यजेत् ।।
(11 - 13 - 29)
यावन्नानार्थघीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः ।
जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ।।
(11 - 13 - 30)
आत्म का संशय-विपर्यय क्या है? मैं शरीर हूँ कि आत्मा-इसका नाम संशय है और अपने स्वरूप आत्मा को कुछ न कुछ मान लेना, यही विपर्यय है। मैं अमुक हूँ-ऐसा मानना ही बंधन है और यही आत्मा का विपर्यय है। इसलिए-विद्वान निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्येस्थितस्त्यजेत् ।। विद्वान को चाहिए कि इस अमुक भाव रूपी बंधन को काटकर 'मैं' जो तुरीय पद आत्मा हूँ, उसमें स्थिर होकर, संसार चिंता का परित्याग कर दे।
यावन्नानार्थघ्धीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः ।
जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ।।
अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रतवत प्रज्ल्पः - भगवान हंस कहते हैं कि महानपुरुषों की युक्तियों के द्वारा नानार्थाकार बुद्धि (अनन्त मान्यतायें) की निवृत्ति जब तक नहीं हो जाती तो यही समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अभी जागते हुए स्वप्न देख रहा है। जहाँ तक इन्द्रियगम्य पदार्थ है वे सभी नानार्थ हैं और अस्तित्व (मैं) आत्मा पर ही आधारित है। अथवा उन सभी विकल्पों का आधार मैं आत्मा हूँ। युक्तियों के द्वारा नानार्थाकार बुद्धि अथवा अध्यास का नाश होता है। कर्ता, क्रिया के बीच जो कुछ भी अमुक भाव है, यह सभी कर्म हैं, ऐसा निश्चय ही महान पुरुषों की युक्ति है। इन युक्तियों द्वारा यदि नानार्थकार बुद्धि की निवृत्ति नहीं हो जाती तो समझो कि वह व्यक्ति जागते हुए कैसे स्वप्न देख रहा है जैसे कि स्वप्नकाल का जागरण।
यावन्नानर्थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः ।
जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ।।
(11-13-30)
'मैं' आत्मा जैसा हूँ वैसा ही हूँ, ऐसा न जानकर कुछ का कुछ मान लेना, यह नानार्थकार बुद्धि है। इस धोखे (अज्ञान) से निवृत्त हो जाना चाहिए। जब सोया हो तो जगाया जा सकता है, परन्तु जो जागते हुए सोया है तो तुम उसके सामने चाहे ढोल पीटो वह जागेगा नहीं, कारण वह सोया ही कहाँ है-ऊपर से खर्राटा ले रहा है, परन्तु भीतर से तो जाग ही रहा है, तो वह कब जागने वाला है-नहीं जागेगा। जिस तरह कोई स्वप्न देख रहा है, तो उस स्वप्न द्रष्टा को स्वप्नावस्था में मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ऐसा भान नहीं होता और जागने पर अपने आप ही कहता है कि आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा। इसी प्रकार इस संसार स्वप्न का द्रष्टा यह नहीं जानता कि मैं संसार स्वप्न देख रहा हूँ। जब संसार स्वप्न से उपरत होगा, तभी वह संसार स्वप्न को जानेगा। क्यों नहीं रामायण के पदों पर ध्यान करते-रामायण तो सभी पढ़ते हो-
उमा कहउं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना ।।
क्यों नहीं इन मंत्रों पर, इन पंक्तियों पर ध्यान देते-जब तक अपने आप में जागा नहीं तब तक उपरोक्त पंक्तियों पर उसकी आस्था नहीं होगी।
अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ।
अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ।।
(गौ.का. अगम-16)
अर्थात् अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोता हुआ जीव जब जागता है तब अपने आपको अजन्मा, अविनाशी, अवस्थाओं से परे, कालातीत जानता है। यानी सारा चराचर 'मैं' आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। यह स्थिति विकल्पगम्य नहीं है। एक तृण को भी अगर अलग मानता है तो वह व्यक्ति अभी मोह निद्रा से जगा नहीं है। वासुदेवः सर्वमिति - आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं
यावन्नानार्थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः ।
जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ।।
(11 - 13 - 30)
असत्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा ।
गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा ।।
(11 - 13 - 31)
यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान्भुङ्क्ते ।।
मस्तकरणैहुँदि तत्सदृक्षान् । स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः
स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदृगिन्द्रियेशः ।।
(11 - 13 - 32)
सुनो-अब भगवान आत्मा की नित्यता का भास, सर्व अवस्था में एकरस है। अब बता रहे हैं-सुनो-
यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान्भुङ्क्ते ।।
समस्तकरणैहुँदि तत्सदृक्षान् ।
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः
स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदृगिन्द्रियेशः ।।
(11 - 13 - 32)
जो भगवान आत्मा 'मैं' सर्व का सर्व, जाग्रत अवस्था के प्रपंच को जानता हूँ, अनुभव करता हूँ वही 'मैं' आत्मा स्वप्नावस्था के प्रपंच को जानता हूँ और सुषुप्ति के आनंद का अनुभव करता हूँ। अरे! मेरे कहने से न मानो। जब तक तुम्हारे हृदय में यह विषय बिल्कुल हृदयङ्गम न हो जाय तब तक न मानो। अनुभव करायेंगे-जो प्रतीति है वह सब 'मैं' आत्मा हूँ-बाकी फिर हरि ॐ तत्सत्। देखो-सबेरे जब तुम सोकर उठे तो तुम्हारी घड़ी में क्या बजे थे? पाँच बजे थे। तो पाँच बजे वाले काल में तुम थे कि नहीं? 'मैं' था, तभी तो पाँच बजे वाले काल को जाना। अब काल बदल रहा है तो काल के साथ ही प्रपंच भी बदलता जा रहा है, क्योंकि प्रपंच कालानुगामी है। परन्तु क्या 'मैं' आत्मा भी बदल जाता हूँ? जी, नहीं, मैं आत्मा नहीं बदलता। सुबह सोकर उठने के बाद जब तक मैं सो नहीं जाता, तब तक जो अवस्था है वह जाग्रत अवस्था कहलाती है। मैं आत्मा जाग्रत अवस्था के प्रपंच को जानता हूँ। स्वप्नावस्था के स्वप्न प्रपंच को मैं आत्मा जानता हूँ, क्योंकि यदि 'मैं' आत्मा न रहूँ तो सुबह उठने पर यह कौन बतलायेगा कि आज मैंने स्वप्न देखा। सुषुप्ति गाढ़ी नींद में समस्त प्रपंचों को समेटकर जब मैं सो जाता हूँ तो 'मैं' आत्मा एकमात्र रह जाता हूँ। तभी तो जागने पर कहता हूँ कि आज जब मैं सोया तो मुझे बड़ा आनंद आया। कहने का मतलब यह है कि तीनों अवस्थाओं का मैं द्रष्टा साक्षी हूँ। तीनों अवस्थाओं में एकरस रहता हूँ इसलिए मुझ आत्मा को तीनों अवस्थाओं की स्मृति रहती है।
एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः ।
संछिद्य हार्दमनुमानसदुक्तितीक्ष्णज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम् ।।
(श्रीमद् भागवत 11-13-33)
ये जो तीन गुण की तीन अवस्थायें हैं-जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति ये मन की हैं, मुझ आत्मा की नहीं। मेरी माया करके, मेरे द्वारा रचित हैं ऐसा निश्चयकर, ज्ञानरूपी खड्ग से सम्पूर्ण संशय, विपर्यय के समूह का नाश कर, अपने स्वस्वरूप भगवान आत्मा में स्थित हो जा-यह जो संसार रूपी वैकल्पिक जाल है, इसको क्या जानो-
ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम् ।
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ।।
(11-13-34)
यह मन का विलास रूप है। दृष्ट विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्-देखो- अलातचक्र कहते हैं कि अधजली लकड़ी को, जिसकी आग बुझी नहीं है और बहुत प्रज्जवलित भी नहीं है-उसे भन्नाटी (भनेटी) के समान घुमाने से अनगिनती चिनगारियाँ निकलती हैं, जिसका प्रकाश चक्र की नाई फैल जाता है-उजाला गोलाकार दिखता है। इसी तरह बुद्धि में मन के विकल्पों का चकाचौंध अलातचक्र के समान संसार घूम रहा है।
ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम् ।
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ।।
(11-13-34)
भगवान कहते हैं कि सिद्ध यानी महानपुरुष जो कि अपने स्वस्वरूप भगवान आत्मा में स्थित है, जो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है, वह इतना उन्मत्त हो जाता है कि जैसे मदिरा पीकर व्यक्ति शरीर पर वस्त्र है या नहीं, इसे भूल जाता है, उसे भान नहीं होता। उसी प्रकार जो सिद्ध पुरुष हैं उन्हें नश्वर शरीर के प्रति आस्था नहीं रहती। शरीर खड़ा है या बैठा है इसका उसे भान नहीं होता। उसका शरीर प्रारब्ध के वशीभूत होता है, जहाँ प्रारब्ध ले जाय।
देहोऽपि दैववशगः खलु कर्मयावत् स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः ।
तं सप्रपञ्चमधिरुढ़समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ।।
(11 - 13 - 37)
सासुः - प्राणः । देह भी जब तक दैववशगः प्रारब्ध के वशीभूत है, तब तक प्रारब्ध जहाँ ले जाय वहाँ चला जाता है। प्राण पर चलता रहता है, परन्तु उस शरीर के प्रति उसकी आस्था नहीं रहती। जो समाधि योग यानी आत्मयोग में स्थित अर्थात् स्वस्वरूपस्थ हैं। उसकी प्रपंच में आस्था वैसे ही नहीं होती जैसे कि जागने पर स्वप्न के प्रति आस्था नहीं रहती। देखो-भैया ! ऊपर जो श्लोक है यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान्- से लेकर यहाँ तक भगवान आत्मा के सत्य, चैतन्य, हंस स्वरूप से जो प्रश्न था उसका उत्तर देते हुए आत्मा की अनुभूति तीनों श्लोकों में समझाये हैं और अभी के श्लोक से भगवान आत्मा 'मैं' क्या नहीं जानता, किसको नहीं जानता। 'मैं' आत्मा सर्व का सर्व, द्रष्टा, साक्षी ज्ञाता हूँ, सर्व की आत्मा हूँ, इसका दिग्दर्शन कराये हैं। भगवान को श्रुति प्रज्ञानघन कहती है। प्रज्ञानघन उसे कहते हैं जो ज्ञानपुञ्ज हो, जिसका ज्ञान ठोस हो, अखण्ड हो। भगवान आत्मा 'मैं' को किसी भी देश, काल, वस्तु को जानने के लिए काल की सीमा नहीं है। जैसा कि इस डंडा (डंडा दिखाकर छुपा लेते हैं) अब इसे जानने के लिए मुझ आत्मा को किनता समय लगा? कुछ तो समय लगना चाहिए। एक मिनट, दो मिनट या 1-2 सेकंड। मैं आत्मा को इसका अनुभव करने के लिए काल की कोई सीमा नहीं है अर्थात् तत्काल ही 'मैं' जानता हूँ इसलिए 'मैं' प्रज्ञानघन हूँ (पू. श्री स्वामीजी ताली पीटकर समझाते हैं) यह शब्द विषय है, अब इसका अनुभव करने के लिए कितना समय लगा? कोई समय नहीं लगा, तत्काल ही 'मैं' इसका अनुभव किया। मुझको किसका ज्ञान नहीं- 'मैं' आत्मा सर्व को जानता हूँ और सर्वकाल, सर्व अवस्था में जानता हूँ इसलिए मैं भगवान आत्मा प्रज्ञानघन हूँ। अब यहाँ पर न्याय दर्शन का कहना है कि वृत्ति और आत्मा दोनों का जब संयोग होता है तब आत्मा किसी चीज का अनुभव करता है, जानता है। जाग्रत अवस्था में रजोगुण की वृत्ति रहती है इसलिए जाग्रत अवस्था के प्रपंच को आत्मा जानता है। स्वप्नावस्था में सतोगुण की वृत्ति रहती है इसलिए स्वप्नावस्था के प्रपंच का आत्मा अनुभव करता है। सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण की वृत्ति रहती है। ऐसा सोया कि मुझे कुछ पता ही नहीं रहा-यही तमोगुण की वृत्ति है। इसके साथ जब आत्मा का संयोग होता है तो सुषुप्ति के आनंद का अनुभव करता है। मूर्छावस्था में दुःखाकार वृत्ति रहती है। समाधि अवस्था में शुद्ध सतोगुण की वृत्ति रहती है। इससे सिद्ध होता है कि बिना वृत्ति के आत्मा किसी भी देश, काल, वस्तु को जानने में समर्थ नहीं है। नहीं तो हमें इसका प्रमाण दो कि बिना वृत्ति के आत्मा किसी देश, काल, वस्तु का अनुभव करता है। लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः न तु प्रतीज्ञावाक्येन-लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, प्रतिज्ञावाक्य से नहीं। तो इस पर वेदांत कहता है कि देखो अनुभव करो-एक वृत्ति अन्तःकरण से उदय हुई और इस शब्द विषयमें आई और दूसरी वृत्ति अभी उदय नहीं है, इन दोनों वृत्तियों की मध्यमावस्था को 'मैं' आत्मा जानता हूँ कि नहीं? जानता हूँ। वृत्ति रहित होकर जानता हूँ या वृत्ति सहित होकर जानता हूँ? वृत्ति रहित होकर जानता हूँ। देखो जाग्रत अवस्था जा रही है और सुषुप्ति अवस्था आई नहीं है, तो इन दोनों संधियों यानी मध्यावस्था को मैं आत्मा जानता हूँ कि नहीं? जानता हूँ। वृत्ति रहित होकर जानता हूँ या वृत्ति सहित? वृत्ति रहित होकर जानता हूँ। यहाँ पर न्याय अपना बोरिया-बिस्तर लेकर भाग जाता है तो इससे सिद्ध होता है कि मुझ भगवान आत्मा को किसी भी देश, काल, वस्तु का अनुभव करने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज का 'मैं' अनुभव करता हूँ तो अनुभव करने के लिए इन्द्रियादिक उपकरणों की जरूरत मुझ आत्मा को नहीं पड़ती। हाँ-उसे अभिव्यक्त (जाहिर) करने के लिए मुझ आत्मा को इन्द्रियों की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब यह कि 'मैं' आत्मा नित्यज्ञान स्वरूप प्रज्ञानघन हूँ।
देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरुपम् ।।
(11 - 13 - 36 )
इस तरह जो स्वरूप में स्थित है उसका दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ।। जैसे मदिरा पीकर व्यक्ति इतना मदान्ध हो जाता है कि उसका वस्त्र भी शरीर से यदि गिर जाय तो उसे इसका भान नहीं होता, उसे होश ही नहीं रहता। इसी प्रकार ब्रह्मानंद रूपी मदिरा को पान करके जो योगी उन्मत्त है, वह संसार से परे रहता है और यदि दैवयोग से उसका शरीर पात भी हो जाय तो उसे इसका भान नहीं होता कि अब यह शरीर न रहा।
खे मध्ये कुरुचात्मानमात्मा मध्ये च खं कुरु ।
सर्वं च खमयं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तय ।।
अपनी आत्मा को आकाश में देखो और आकाश को अपने 'मैं' आत्मा में देखो। सारे चराचर को आकाशमय करके कुछ भी चिंतन न करो-जाग्रत अवस्था स्वप्न में नहीं, स्वप्नावस्था सुषुप्ति गाढ़ी नींद में नहीं, सुषुप्ति अवस्था जाग्रत और स्वप्न में नहीं। इन अवस्थाओं का एक-दूसरे में व्यभिचार है, परन्तु 'मैं' आत्मा इन तीनों अवस्थाओं में एकरस रहता हूँ। मुझ भगवान आत्मा का इन अवस्थाओं में अव्यभिचार है। ऐसा जिसको निश्चय है वही स्थितप्रज्ञ है, वही बंधन से मुक्त है। फिर उसे संसार स्वप्न के प्रति आस्था नहीं रहती। इस प्रकार हंस रूप में भगवान ने सनकादिक ऋषियों को उनके प्रश्नों का उत्तर देकर आत्मतत्व का साक्षात्कार कराया। यही हंसोपाख्यान है और इस समय की कथा का यहीं उपसंहार है।
श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव ।।
सप्तम दिवस
परीक्षित मोक्ष
24-2-1969, प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
अनन्त नाम, रूपों में अभिव्यक्त, अहमत्वेन प्रस्फुरित, महामहिम स्वात्म- स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित आत्मजिज्ञासुगणः -
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।।
(कठो.)
अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वालों भव्य जीवो ! 'उत्तिष्ठत'-उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष के उपसन्न होकर अपना आत्मकल्याण करो-अनन्त जन्मों के पूर्वार्जित पुण्य उदय होने पर यहाँ पर श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता के माध्यम से आत्मतत्व का निरूपण हो रहा है जिसकी आज पूर्णाहुति है। जिस समय योगेश्वर भगवान की कृपा से महाभागवत श्री उद्धव को आत्म साक्षात्कार हो गया, उसी समय भगवान को उद्धवजी दण्ड प्रणाम कर द्वारिकापुरी छोड़कर बदरिकाश्रम को चले गये। भगवान द्वारिकापुरी से यदुवंशियों को लेकर प्रभासक क्षेत्र पहुँचे। वहाँ पर ब्राह्मणों के अभिशाप के कारण यदुवंशीगण मदिरापान करके उन्मत्त हो गये और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपसमें राग-द्वेष बढ़ा और घोर महायुद्ध हुआ, फिर कौन किसको जानता है, आपस में सब लड़ मरे-प्रभु की जैसी इच्छा- भगवच्छिा गरीयसी। भगवान बलराम जी यदुवंशियों को समझाने के लिए उठे, परन्तु उनकी भी किसी ने न सुनी, उन्होंने श्री बलराम जी पर ही आक्रमण शुरू कर दिये। तो क्रोध में बलरामजी हल-मूसल लेकर दौड़े और यदुवंशियों का संहार हो गया। इसके बाद ही श्री बलराम जी भी अपनी योगलीला समाप्त कर दिये। भगवान श्रीकृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे एक चरण दूसरे पर रखकर बैठे थे, तो जरा नामक व्याध ने भगवान के कमल- चरणों की रेखाओं के दिव्य प्रकाश को मृग की आँख की ज्योति समझकर बाण मारा। लीला समाप्ति का कोई न कोई निमित्त कारण होता है। बाद में जब व्याध आया और देखा तो उसे बहुत दुःख हुआ और उसने क्षमा प्रार्थना की। जब परमधाम जाने लगे तो भगवान ने सारथी के हाथ संदेश भेजा कि द्वारिकापुरी में जो यदुवंशी रह गये हैं, उन्हें कह देना कि यहाँ जो यदुवंशी आये थे वे मर गये और तुम लोग द्वारिकापुरी छोड़ दो। कारण, द्वारिकापुरी आज के सातवें दिन जलमग्न हो जायेगी। इसलिए शीघ्र से शीघ्र द्वारिकापुरी छोड़कर बाहर निकल जायें। अब मैं अपनी योगलीला समाप्त करूंगा और मेरे संकल्प द्वारा निर्मित जो द्वारिकापुरी हैं वह समुद्र में डूब जाएगी। मेरे ही संकल्प से यह पुरी समुद्र के बीच निर्मित हुई थी। अब वह नहीं रहेगी। भगवान श्रीकृष्ण उन्हीं यदुवंशियों को प्राभसक क्षेत्र ले गये थे जो सोलह हजार एक सौ आठ रानियों से उत्पन्न हुए थे और बाकी सब द्वारिकापुरी में ही थे। जब भगवान परमधाम जाने के लिए प्रस्तुत हुए तो ब्रह्मादिक देवता आकाश मंडल से नीचे उतरे और स्तुति करने लगे। उसी समय देवताओं के ही मंडल में भगवान ने अपनी योगलीला समाप्त कर दी। तत्पश्चात् भगवान के परमधाम जाने के बाद ही कलिकाल आ गया। श्री स्वामी शुकदेव जी फिर आगे जो यदुवंशी और अनेकानेक राजे-महाराजे होंगे उनका वर्णन किये हैं। किसका राज्य कितने वर्षों का होगा और उनके पुत्र-पौत्र कितने दिन राज्य करेंगे आदि वर्णन किये हैं। स्वामी शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं-यह बारहवें स्कन्ध के पाँचवें अध्याय में वर्णित है-
अत्रानुवर्ण्यतेऽभीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्हरिः ।
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः ।।
(12 - 5 - 1)
राजन् ! आज तो श्रीहरि भगवान विश्वात्मा को ही मैं कह रहा हूँ। अब कथा भाग नहीं रहा, सब सुना चुका।
अत्रानुवर्ण्यतेऽभीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्हरिः ।
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः ।।
(12-5-1)
त्वं तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि ।
न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नङ्ङ्क्षयसि ।।
(12 - 6 - 2)
परीक्षित ! अभी तक जो तू अपने आपको छः उर्मियों वाला शरीर मानकर जन्म मरण वाला मानता था, यह तेरी महान भूल है, ऐसी पशुबुद्धि का नाश कर। तू भगवान आत्मा न जन्मा है और व भविष्य में मरेगा। निम्नलिखित शरीर की उर्मियाँ हैं-जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणते, अपक्षीयते, मृयते-गर्भाधान होता है, पैदा होता है, बढ़ता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, मरता है। ये छः उर्मियाँ विकार-शरीर की है, मैं आत्मा की नहीं। जब मैं शरीर के धर्मों को अपना धर्म मान लेता हूँ तब मैं वर्णी हूँ, आश्रमी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बालक, युवा, वृद्ध हूँ इत्यादि मानता हूँ। जब अपने आपको जीव मानता हूँ तब जीव के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करता हूँ कि मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ, स्वर्गी-नरकी हूँ, धर्मी-अधर्मी हूँ, पुण्यी-पापी हूँ, बद्ध-मुक्त हूँ, ज्ञानी-अज्ञानी हूँ आदि। इस धारणा को पशुबुद्धि कहते हैं, तो इस पशुबुद्धि का अब नाश कर। आज के पहिले भी तू था और आगे भी रहेगा, तेरा कभी नाश नहीं है। इस पर टिक जा- आज के पहिले पैदा नहीं हुआ था और न आगे मरेगा-ये सब पशु बुद्धि की धारणायें हैं।
त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि ।
न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नङ्क्षयसि ।।
(12 - 6 - 2)
देह के नाश हो जाने से जीवात्मा का नाश नहीं होता। इसलिए परीक्षित ! तू यह जान ले, इस समय इसका अनुभव कर-
न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् ।
बीजाङ्कुरवद् देहादेव्र्व्यतिरिक्तो यथानलः ।।
(12-5-3)
यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोऽमरः ।।
(12 - 5 - 4)
स्वप्न में स्वप्नदृष्टा देख रहा है कि उसका सिर कट गया है, तो भला बताओ जिसका सिर कट गया है क्या वह अपने कटे हुए सिर को देखेगा? स्वप्ननर का सिर कटा है, स्वप्नद्रष्टा का नहीं। उस कटे हुए सिर को जो देखता है, अनुभव करता है, वही अजर-अमर आत्मा अवाङ्गमनसगोचर तू है।
घटे भिन्ने यथाऽऽकाश आकाशः स्याद् यथा पुरा ।
एवं देहेमृत जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ।।
(12-5-5)
परीक्षित् ! घड़े के फूट जाने से घड़े के अंदर का जो पोल आकाश है वह कहीं नहीं जाता, क्योंकि कहीं बाहर से आया नहीं है, वह महाकाश हो जाता है। क्योंकि वह अभिन्न है, घटाकाश महाकाश एक ही है। इसी तरह शरीर और जीवात्मा को समझो। शरीर के छूट जाने पर जीवात्मा कहीं नहीं आता जाता, वह तो परमतत्व है, परमात्मा है। इसलिए परमात्मा हो जाता है, क्योंकि वस्तु का कहीं आना-जाना नहीं है।
चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः ।
मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम् ।।
(12-5-10)
विप्रवाक्येन चोदितः प्रेरितः तक्षकः सर्पः मृत्यूनांमृत्युमीश्वरम् त्वां आत्मानं न धक्ष्यति। ब्राह्मण वाक्य द्वारा प्रेरित तक्षक सर्प अभी डसने आयेगा, उस समय तू यही धारणा करना कि मुझ अजर, अमर, अविनाशी भगवान आत्मा को तक्षक नहीं डसेगा, क्योंकि मैं कालों का काल महाकाल भगवान आत्मा हूँ। कैसे? जब तुम आज सोकर उठे तो घड़ी में क्या बजा था। मान लो 5-6 बजे था, तो 6 बजे नाम के काल को 'मैं' ने भक्षण कर लिया। 'मैं' नहीं खाया तो फिर और किसने उस 6 बजे वाले काल को खाया? 'मैं' ने। यदि 'मैं' आत्मा 6 बजे न होता तो 6 बजे के काल को 'मैं' कैसे जानता? तो 6 बजे को खाया 7-8-9 कालों को खाया-चतुर्युग सहस्त्राणि दिनमेकं पितामह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, ये चारों युग जब एक हजार बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। हजार चौकड़ी युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा की इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। इस तरह ब्रह्माजी सौ वर्ष के हो जाते हैं। इस तरह ब्रह्माजी सौ वर्ष के हो जाते हैं तो फिर ब्रह्माजी भी लुढ़क जाते हैं। फिर दूसरे ब्रह्मा पैदा होते हैं। अभी जो समय चल रहा है उसे ब्राह्मण विद्वान संकल्प में क्या पढ़ते हैं-द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे-ब्रह्माजी अब अधेड़ हो गये हैं। 50 वर्ष ब्रह्माजी का बीत चुका है। 51 वें वर्ष का पहला दिन है और सिर्फ दस बजा हैं। इसे दूसरा प्रहर कहते हैं। जिस तरह तुम्हारे यहाँ के दिन को सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि कहते हैं इसी तरह ब्रह्माजी के दिन को कूर्म कल्प, मत्स्य कल्प, वाराह कल्प इत्यादि कहते हैं। ब्रह्माजी के इस दिन का नाम वाराह कल्प है। ब्रह्माजी के इसी कल्प में भगवान का वाराहावतार हुआ था। इसलिए जब ब्रह्मा का दिन होता है तो रात्रि भी होती है और जब दिन, रात है तो उसका नाश भी है। काल तो ब्रह्माजी को भी नहीं छोड़ता, खा जाता है। किसी को नहीं छोड़ता और इसका वेग इतना तेज है- गति इतनी प्रखर है कि धड़ाधड़ वर्तमान भूत हो रहा है और भविष्य वर्तमान-
जो कालहू कर काल भयंकर। वरनत उमा शारदा शंकर ।।
तो 'मैं' ने 8 बजे को खाया, 9-10 बजे को खाया। परन्तु मुझ आत्मा भगवान को खाने वाला कोई नहीं है। परीक्षित् को इस प्रकार बोध कराकर-
चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः ।
मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम् ।।
(12 - 5 - 10)
इसलिए तू मृत्युओं का मृत्यु महाकाल भगवान आत्मा है। अस्तु-ब्राह्मण वाक्य द्वारा प्रेषित तक्षक आयेगा तो तुझे नहीं काटेगा क्योंकि तू तो महाकाल है।
दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननैः ।
न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः ।।
(12-5-12)
अभी तक्षक जीभ लपलपाता हुआ आयेगा, उस समय किस धारणा में स्थित होना। तू क्या निश्चय करना-जितने भी मरने वाले बैठे हो, अरे ! शंका मत करो-जितने भी पैदा होते हैं सभी काल कलेवा होते हैं, मरते हैं। मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसी भावना किस हृदय में उठती है? तो मरने वाले बैठे हो कहे तो क्या बुरा कहे। स्वामी शुकदेव जी महाराज परीक्षित् को अनुभव करा रहे हैं- अभी तक्षक जीभ लपलपाते हुए तुझे डसने आयेगा तो तू क्या निश्चय रखना, किस सिद्धांत में स्थित रहना कि मैं भगवान आत्मा हूँ। शरीर को और समस्त विश्व प्रपंच को अपने स्वरूप भगवान आत्मा से भिन्न नहीं देखना। यही अंत समय यानी मृत्यु काल की धारणा है। आत्मैवेद् सर्वम् - मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से जब एक कण भी भिन्न नहीं है, तो काल भी तो 'मैं' ही हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि पहिले तो शरीर से भिन्न करके आत्मा को बताया गया और बाद में कहते हैं कि शरीर भी 'मैं' ही हूँ। तो देखो पहले श्लोक में अन्वय है और दूसरे श्लोक में व्यतिरेक है। पहले श्लोक में कहते हैं कि शरीर के नाश हो जाने पर, देही जो जीवात्मा है उसका नाश नहीं होता इसलिए शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ-शरीर से अलग आत्मा को जानना और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि अपने स्वरूप भगवान आत्मा से विश्व (प्रपंच) को अलग नहीं देखना ? यही अनुभव करना कि शरीर और विश्व (प्रपंच) भी मैं आत्मा ही हूँ। शुरू में कहे, शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ-यह वेदांत की प्रक्रिया है, इसे अन्वय कहते हैं। शरीर भी 'मैं' हूँ-इसे व्यतिरेक कहते हैं। यह वेदांत का सिद्धांत है और शरीर तीन काल में है ही नहीं, 'मैं' ही 'मैं' हूँ-यह वेदांत है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि पहिले तो शरीर से भिन्न करके आत्मा को बताया गया और बाद में कहते हैं कि शरीर भी 'मैं' ही हूँ। तो देखो पहले श्लोक में कहते हैं कि शरीर के नाश हो जाने पर, देही जो जीवात्मा है उसका नाश नहीं होता इसलिए शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ-शरीर से अलग आत्मा को जानना और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि अपने स्वरूप भगवान आत्मा से विश्व (प्रपंच) को अलग नहीं देखना? यही अनुभव करना कि शरीर और विश्व (प्रपंच) भी मैं आत्मा ही हूँ। शुरू में कहे, शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ-यह वेदांत की प्रक्रिया है, इसे अन्वय कहते हैं। शरीर भी 'मैं' हूँ-इसे व्यतिरेक कहते हैं। यह वेदांत का सिद्धांत है और शरीर तीन काल में है ही नहीं, 'मैं' ही 'मैं' हूँ-यह वेदांत है। शिव ! देखो, अब तीनों का अंतर-पहिले प्रक्रिया, फिर सिद्धांत और फिर वस्तु (वेदांत) । देखो, सुनो ध्यान से-यह आखिरी उपदेश है-बड़ी सरलता के साथ समझायेंगे। सोना है- तो सोना पीला होता है, मुलायम होता है और वजनदार होता है। पीला, वजन, मुलायम ये तीन लक्षण जिसमें हो उसे सोना कहते हैं। यदि सोना अपने पीलापन को, वजनपने को, मुलायनपने को यानी अपने स्वरूप को भूल जाये और अपने को कर्णफूल, बाली, टॉप्स, कंगन, लाकेट, चूड़ी, अंगूठी, चेन इत्यादि आभूषण माने तो यह सोने का अज्ञान है। सोना अपने वजनपन, पीलापन और मुलायमपने को भूलकर अपने आपको आभूषण मानने लगे, तो क्या वह सोना रहेगा? सोने का आभूषणाभिमान हटाने के लिए उसे अपने स्वरूप का अनुभव करना होगा कि वह पीला, वजनदार और मुलायम है। उस सोने से यही कहना होगा कि ऐ सोना। जिस आभूषण को तू अपना स्वरूप मानता है वह तू नहीं है, उसको आभूषण से अलग करके बताना पड़ेगा कि तू आभूषण नहीं वरन पीला, वजनदार एवं मुलायम तीन लक्षणों वाला सोना है, यही तेरा असली स्वरूप है-यही प्रक्रिया है। अब चलो सिद्धांत समझायें। ऐ सोना ! देख तुझ स्वर्ण के बिना क्या आभूषण है और जब नहीं है तो आभूषण भी तू सोना ही है-यही सिद्धांत है। अब वस्तु का अनुभव करायें। ऐ सोना ! क्या तुझ स्वर्ण देश में आभूषण है? आभूषण तो तेरे स्वरूप में तीन काल में है ही उनहीं-यही बोध है। तो सर्व भगवान है, सिद्ध हुआ। भगवान देश में सभी भगवान है यह बोध है। भगवान देश में सब पदार्थ आधारित है-अब यह प्रक्रिया है। अहमस्मि- मैं हूँ-यह बोध है, वेदान्त है। पहिले प्रक्रिया और समझायेंगे। पहिले भी यहाँ पर जब चतुःश्लोकी भागवत का निरूपण किया गया उस दिन भी प्रक्रिया समझाई गई थी परन्तु उस समय इतने लोग नहीं थे इसलिए आज और समझायेंगे। इतने हृदय उस समय नहीं थे-यह आखिरी दिन है, फिर समझ लो। मैं और मेरा, ये दो शब्द हैं। इन शब्दों का अर्थ एक ही नहीं होता। मेरा संबंधवाचक शब्द है और मैं कर्तृवाचक। स्वयं अपने आपके लिए 'मैं' कहते हो और अपने से संबंधित पदार्थ के लिए मेरा कहा जाता है। इसलिए 'मैं' का मतलब मेरा नहीं और मेरा मतलब 'मैं' नहीं-इसको खूब समझ लो। जब कहता हूँ मेरी साइकिल, मेरा घर, मेरा डण्डा, तो यदि मेरा का अर्थ मैं हो तो मैं साइकिल हो जाऊँ, घर हो जाऊँ, डण्डा हो जाऊँ। इसलिए मेरा का अर्थ 'मैं' नहीं होता। मेरा उसके लिए होता है, जिससे अपना संबंध होता है। भैया ! मेरा नाम देवदत्त, यज्ञदत्त, जमुनाप्रसाद, मनोहरलाल है तो मेरा होने के नाते मैं देवदत्त, यज्ञदत्त, जमुनाप्रसाद आदि नहीं हूँ। नाम तो पैदा होने के बाद रखा जाता है। यदि पहले से ही मेरा नाम देवदत्त होता तो जब मैं पैदा हुआ तभी घर के लोग कहते-भाई ! दौड़ो, देवदत्त पैदा हुआ है परन्तु ऐसा नहीं होता। मेरा नाम देवदत्त है, इसलिए नाम से मैं अलग हुआ। मेरा का अर्थ 'मैं' नहीं होता। तो मेरा हाथ कहने से ही मालूम होता है कि मैं हाथ, पैर, शरीर आदि नहीं हूँ और मैं शरीर भी नहीं, शरीर तो पंचमहाभूतों का कार्य है। जिस प्रकार मकान ईंटा, चूना, गारा से बनता है। इसी तरह शरीर भी मांस, मज्जा, रक्त आदि से बना है। जिस तरह मकान में खम्भे होते हैं वैसे ही इस शरीर रूपी मकान के हाथ पैर खम्भे हैं। मकान में बल्लियाँ लगी रहती हैं, शरीर में हड्डी रुपी बल्लियां लगी है। मकान में दरवाजे होते हैं तो इस शरीर में नौ दरवाजे होते हैं। मकान घास-फूस से छाते हो तो यह शरीर चमड़ी से छाया गया है। जैसे मकान पीला, लाल, सफेद आदि रंग से पोता जाता है वैसे ही यह शरीर भी मकान की नाई कोई गोरा, तो कोई काला, तो कोई साँवला है और जैसे 'मैं' मकान नहीं वैसे ही 'मैं' शरीर नहीं। हाँ-शरीर में रहने की गरज से 'मैं' कहता हूँ कि यह मेरा शरीर है। तो न 'मैं' शरीर हूँ, न मेरा शरीर है। शरीर पंचभूतों का कार्य है, मल, मूत्र का भांड है, माता-पिता के रज, वीर्य से बना है। इसे अच्छी तरह समझ लो। जब 'मैं' शरीर न मेरा शरीर और यह शरीर ही बालक, युवक और वृद्ध होकर नाश हो जाता है। तो शरीर ही उत्पन्न होता है और शरीर ही मर जाता है। 'मैं' तो ज्यों का त्यों हूँ। शरीर मरता है तो 'मैं' मरता हूँ, यह तुम्हारी समझ गलत है। शरीर घटता, बढ़ता है 'मैं' नहीं। जैसे किसी मित्र के साथ तुम किसी के घर गये तो वह तुमसे पूछता है कि साथ में जो महाशय आये हैं उनकी क्या तारीफ है, 'मैं' इनको नहीं पहचानता। तो तुम कहते हो कि ये मेरे बचपन के साथी हैं। 'मैं' इनके साथ प्रायमरी पढ़ा, हाईस्कूल पास किया, कॉलेज में पढ़ा। जब अपने मित्र के साथ तुम प्रायमरी में पढ़ते थे, तो क्या तुम ऐसे ही थे जैसे अब हो? क्या उस समय भी तुम्हारी दाढ़ी, मूँछ थी? तो उस समय तुम्हारा और तुम्हारे मित्र का शरीर छोटा-सा था। तो, शरीर ही तो बदला। यदि 'मैं' शरीर होता तो मैं आत्मा भी बढ़ा होता, बदल जाता। तो फिर यह याद किसको रहती कि बचपन में 'मैं' इसके साथ पढ़ा था। तो शरीर बढ़ता-घटता है, 'मैं' नहीं। नहीं तो मैं आत्मा भी शरीर के साथ फिर बुड्ढ़ा हो जाता। शरीर के मरने से 'मैं' आत्मा मरता नहीं। 'मैं' किसी का नहीं और न कोई मेरा है। तो इसी तरह 'मैं' न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शुद्र, न संन्यासी, न उदासी, न निर्वाणी, न निर्मोही, न राधास्वामी, न वल्लभी, न प्रणामी, न जयकृष्णी, न मुसलमान, न ईसाई, न यह पंथी, न वह पंथी। अभी भारत में दो हजार नौ सौ निन्यानबे पंथ हैं और दिन-प्रतिदिन बनते ही जा रहे हैं। आपस में न बनी, चलो एक पंथ और निकल गया। तो हमें कोई पंथ नहीं बनाना है। अलग-अलग पंथ निकलते चले जा रहे हैं। खैर, ये सब पंथ-पंथाई शरीर से संबंधित हैं और न 'मैं' शरीर, न मेरा शरीर। तो फिर क्या मैं मन हूँ? मेरी बुद्धि कहता हूँ इसलिए मैं बुद्धि में भी नहीं। क्या मैं प्राण हूँ? नहीं। मेरा प्राण कहता हूँ इसलिए मैं प्राण नहीं। तो, न मैं शरीर, न नाम, न हाथ-पैर, न मुँह, न मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण ये सब संबंधवाचक हैं। कहते हो-मेरी आत्मा-हालांकि आत्मा शब्द स्वयं के लिए आता है, मेरी आत्मा कहना ठीक नहीं है। परन्तु चलो तुम्हारी ही बात सही-मेरी आत्मा। तो अब क्या बचा? 'मैं'। तो, 'मैं' क्या चीज हूँ-इसको प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया की आवश्यकता इसलिए है कि अनादिकाल से यह धारणा बन रही है कि मैं साढ़े तीन हाथ का शरीर हूँ। इस अज्ञान का नाश करना जरूरी है करके प्रक्रिया समझाई जाती है- कि 'मैं' शरीर नहीं, न मेरा शरीर है, 'मैं' आत्मा हूँ। दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता-जब तक कि मन्थन न किया जाये। तो यह प्रक्रिया मन्थन करना है। मैं आत्मा सर्व में ओत-प्रोत हूँ, रग-रग में हूँ-तो अभी विचार रूपी मथानी से मन्थन कर रहे हैं-विचार करने से शरीर से मैं आत्मा अलग हो जाता हूँ। सुनार सोने को गलाकर खोट भाग अलग और खरा भाग अलग करता है। जिसको मेरा कहते हैं-वह खोट है, उसको अलग करो और 'मैं' को ग्रहण कर लो। मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, अब बाकी क्या बचा? 'मैं'। चलो, विचार करें कि 'मैं' क्या हूँ? अच्छा एक बात और सुन लो-स्वामी जी अपने 'मैं' को 'मैं' कहते हैं तो क्या मेरा 'मैं' स्वामीजी के 'मैं' से अलग है? नहीं। समझ लो कि जो 'मैं' इस समय गद्दी से आत्मा का ज्ञान करा रहा है, उपदेश कर रहा है, तत्व का बोध करा रहा है, वही 'मैं' आत्मा सर्व स्थानों से सुन रहा है। हाँ, शरीरों का भेद है। सर्व का सर्व आत्मा एक का एक ही है। जो सब में समान रूप से प्रस्फुरित है। चलो-सब शरीर से जो 'मैं' सुन रहा है, वही 'मैं' एक शरीर से उपदेश कर रहा है। ये सारे शरीरों में 'मैं' एक हूँ। समझो ! कभी शरीर में कहीं दर्द हो जाय, कांटा लग जाय, सिर में दर्द हो जाये तो 'मैं' सब स्थानों से दर्द को जानता हूँ। पैर का दर्द पैर से, सिर का दर्द सिर से। 'मैं' शरीर में यदि एक जगह होता तो शरीर के उसी भाग के दर्द को जानता-जिसमें 'मैं' होता, परन्तु 'मैं' सारे शरीर में व्यापक हूँ इसलिए शरीर के सभी भागों के दुःख-सुख को जानता हूँ, अनुभव करता हूँ।
ॐ !!!
***
महर्षि मुक्त.
महर्षि मुक्त जैसे थे वैसे ही थे। यदि यह कोई दावा करे कि ऐसे थे और वैसे थे, तो उनका दावा एकदम गलत ही होगा। अपने परिचय में वे स्वयं कहा करते थे कि हैं तो हम अजन्मा लेकिन हमें आप लोगों के खातिर आना पड़ा।
उन्होंने यह भी कहा था कि " भगवान को तो जान सकते हो क्योंकि तुम्हारा आत्मा है परन्तु मुक्त को समझना बहुत ही कठिन है (सम्भव नहीं)" आत्मा का लक्षण होता है परन्तु इनका तो कोई लक्षण ही नहीं था। ऐसे अलक्षण को यदि कोई जान, जाय तो बन्ध्या का पुत्र सिंह का शिकार कर सकता है।
अपने पचास वर्षों के अनवरत प्रचार में जिस सिद्धांत या धर्म की इन्होंने प्रतिष्ठा की उस धर्म को महात्मा करपात्री जी ने 'ज़िन्दा वेदान्त' कहा है और यह भी कहा उन्होंने कि अभी विश्व में ज़िन्दा वेदान्त (सत्य धर्म) का प्रचार कोई कर रहे हैं तो वे महर्षि मुक्त ही हैं।
• शास्त्रों ने इनका परिचय इस प्रकार दिया है-
यस्यान्तं नादि मध्यं नहि कर चरणं नाम गोत्रं न सूत्रम्,
नो जातिर्नैव वर्णाः नहि भवति पुरुषो न नपुंसो न च स्त्री।
नाकारं नैवकारं नहि जनि मरणं नास्ति पुण्यं न पापम्,
तत्वं नो तत्वमेकं सहज समरसं, सदगुरूं तन्नमामि ।
प्रकाशक
महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति
मुख्यालय-आनन्द भवन, 61/152, बंधवापारा,
पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.)
www.maharshimukta.org