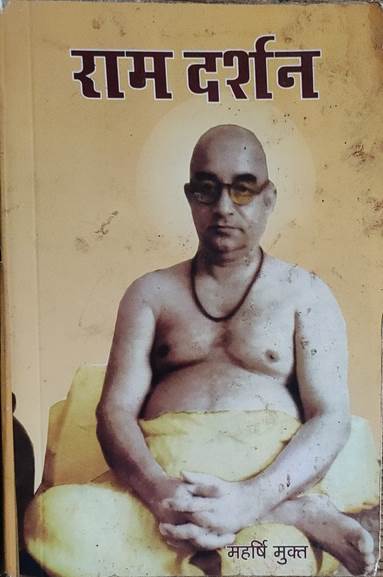
राम दर्शन
(सम्पूर्ण)

महर्षि मुक्त
राम दर्शन
निरूपणकर्ता -महर्षि मुक्त
प्रकाशक -महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति केन्द्र, दुर्ग (छत्तीसगढ)
(सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशकाधीन)
मुद्रक -महावीर ऑफसेट रायपुर (छत्तीसगढ) फोन: 0771-255140
डाटा एन्ट्री -नेचर ग्राफिक्स शांति चौक, पुरानी बस्ती, रायपुर मो. : 9302230478
तृतीय संस्करण -25 जुलाई 2010 (गुरु पूर्णिमा)
प्रति -1000
कार्यालय एवं पुस्तक -डॉ. एस.एन. त्रिपाठी 50/152, बंधवापारा, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.) - मिलने का पता 492001 मो. : 9926130014
मूल्य -250/- (दो सौ पचास रुपये मात्र)
तृतीयावृत्ति पर संक्षिप्त उद्बोधन
प्रिय अभेद आत्मन्, रामदर्शन की तृतीयावृत्ति की प्रस्तुति पर समिति मुदित है, इस आवृत्ति में प्रस्तुत साहित्य का कलेवर परिवर्तन ही किया गया है। विषयवस्तु ज्यों का त्यों है, अपितु इस संस्करण में एक नये प्रसंग का समावेश जरूर किया गया है, वह है महारानी शतरूपा द्वारा मांगा गया सहज वरदान -
सो सुख सो गति सो भगति सो निज चरन सनेह ।
सो विवेक सो रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहू ।।
वैसे तो रामायण पर विद्वान महापुरुषों द्वारा 400 वर्षों में अनेक टीकाएँ हुई हैं, परन्तु वर्तमान में इनके मंत्रों पर जो अलौकिक भाष्य हुए हैं, उन दुर्लभ भाष्यों को प्रकाशित कर आप तक पहुँचाकर समिति धन्य हो रही है।
जिस तरह गीता के अर्थ (भाव) को कृष्ण ही जानता है, उसी तरह से रामायण के भावों को सिवाय राम के किसी अन्य में ताकत नहीं जो इसे जान सके, तभी तो कहा गया है कि- किमि समुझै, यह जीव जड। प्रस्तुत साहित्य में भगवान राम के भावों को ज्यों का त्यों बताया गया है, शर्त इतनी है कि इन भावों को "शिव" होकर ग्रहण करें न कि जीव होकर और तभी उसका ग्रहण भी संभव होगा।
श्री रूपेन्द्रनाथ तिवारी (रामावतार भाई) ने इस पुस्तक के संशोधन में जो अपना अमूल्य समय एवं परिश्रम दान किया है, इसके लिए समिति उनका आभारी है। श्री झग्गर सिंह देवांगन जी को धन्यवाद, जिनके सौजन्य से मनु शतरूपा वरदान प्रसंग प्रस्तुत पुस्तक में शामिल किया गया। प्रूफ रीडिंग में श्री महेन्द्र आडिल एवं श्री बसंत पुरी गोस्वामी का सहयोग स्तुत्य है। समिति इनके भी आभारी है। पं. श्रीरामलाल जी शुक्ल का अमूल्य सहयोग वंद्य है। दाऊ गोकुल बंछोर का प्रयास प्रशंसनीय है।
देवमाता, सुरसा के मुख के समान बढ़ती महंगाई के कारण प्रकाशन में कठिनाई आ रही है, फिर भी आपकी जिज्ञासा शान्ति हेतु समिति अपना गिलहरी प्रयास सतत् बनाई हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में मूल्य संबंधी या अन्य कोई त्रुटि विद्वान पाठकों को अनुचित लगे तो उनसे करबद्ध क्षमा की कामना सहित -
सत्यानंद
व्यक्ति परिचय
देनहार कोऊ और है देवत है दिन रैन ।
नाम लेत रहिमन को ताते नीचे नैन ।
एक ऐसा व्यक्ति, जिसके लिए यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थ हो रही है। जिनने अत्यंत संकोचपूर्वक इस विवरण को प्रकाशित करने की हमें सहमति प्रदान की है -
नाम -श्री यादोराम गंगबेर
आत्मज -श्री सदवाराम गंगबेर
माता -श्रीमती मानबाई
जन्मतिथि -17 अप्रैल 1950
योग्यता -बी.एस.सी.
जन्म स्थान -बगदेई, पो.-लिमोरा, तह.-गुरुर (छ.ग.) जिला-दुर्ग
व्यवसाय -आप एक सम्पन्न कृषक हैं, कृषि आपका पैतृक व्यवसाय है
अन्य रुचि -आप सेवाभावी एवं बैद्यक में रुचि रखने के कारण स्वयं
जड़ी-बूटियों से दवा तैयार करके अनेक जटिल रोगों
का उपचार करते हैं.
आप स्वभाव से अत्यंत विनम्र एवं संत सेवी होने के कारण गृहस्थ जीवन को अंगीकार नहीं किया। आप महर्षि मुक्त के कृपा पात्र हैं।
आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य सत्पुरुषों की सेवा करना एवं उनके सत्संग का लाभ लेना है। महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति के आप संरक्षक सदस्य एवं समिति के समर्पित सदस्य हैं। अपने इसी स्वभाव से प्रेरित होकर इन्हें प्रस्तुत ग्रंथ 'रामदर्शन' की इस आवृत्ति प्रकाशनार्थ 'पचपन हजार रुपये' की सहयोग राशि समिति को प्रदान करके अनुगृहीत किया है।
हम उनके इस अपूर्व योगदान के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते, उन्हें साधुवाद देते हैं।
आशा है, उनकी यह दानशीलता अन्य श्रेष्ठिजनों के लिए श्लाघनीय एवं अनुकरणीय सिद्ध होगी। अलं !
भवदीय
अध्यक्ष
महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति
प्रस्तावना
गोस्वामी तुलसीदास का 'रामचरित मानस' एक अद्भुत आध्यात्मिक ग्रंथ है। न केवल इसलिए कि वह शताब्दियों से भारतवासियों के बहुत बड़े वर्ग में सबसे अधिक पठनीय ग्रंथ रहा है वरन, इसलिए भी वह शिक्षित-अशिक्षित, विद्वत- अविद्वत, गृहस्थ-संन्यासी, संत-सामान्य जैसे विषमवर्गीय समूहों में समरूपेण समाहत हुआ है। उसमें रामकथा के सुपरिचित ऐतिहासिक बिम्बों के सहारे भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, धार्मिक लोक-जीवन, नीतिपरक आचरण को पुरुषार्थमय मानव जीवन में इस तरह गूंथकर रखा गया है कि सभी परिस्थितियों में लोग सहज ही उसमें अपने अस्तित्व का अर्प ढूँढ़ लेते हैं। घर-गृहस्थी की झंझटों में फँसे सामान्यजन फुरसत के समय उनके पठन-श्रवण से परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर चिंतनशील और दृष्टि सम्पन्न विद्वतजन उसी 'रामचरितमानस' की गहराई में उतरकर उसमें समाये उन ऊँचे आध्यात्मिक शिखरों की खोज करते हैं जिन्हें उसके प्रभूत शब्द-राशि ने अपने अंतर में छिपा रखा है। उनकी ऐसी खोज हमें बार-बार चमत्कृत करती है। महर्षि मुक्त का 'रामदर्शन' इसी तरह का चमत्कार पैदा करने वाली 'रामचरितमानस' की व्याख्या है।
ऐसा नहीं है कि रामकथा का आध्यात्मिक निरुपण पहली बार हुआ है। 'रामचरितमानस' के बहुत पहले ही 'अध्यात्म रामायण' के विस्तारपूर्वक रामकथा का यह रुप निखारा जा चुका है। किंतु महर्षि मुक्त की व्याख्या में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहली यह कि उन्होंने रामकथा के आध्यात्मिक गूढ़ाशय को तुलसीदास के शब्दों में से ही ढूंढ निकाला है, यद्यपि अपने प्रकट अर्थ में भी वे शब्द उतने ही मर्मस्पर्शी और प्रभावोत्पादक हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकट शब्दार्थों के नीचे जिस आध्यात्मिक शिखर की खोज उन्होंने की है वह नया और निराला है। 'आध्यात्म रामायण' हमें 'भगवद्गीता' की आध्यात्मिकता की याद दिलाता है। कृष्णावतार में साकार ब्रह्म रुप कृष्ण अपने चरित और शब्दों में ब्रह्म की निराकारता की झलक दिखाते हैं और इसलिए 'लीला पुरुषोत्तम' कहे जाते हैं। दूसरी ओर 'रामचरितमानस' में चित्रित रामावतार में राम के चरित और शब्दों में नहीं वरन् उनकी 'मर्यादा' का 'नीतिमत्ता' के आवरण में से निराकार ब्रह्म की झलक दिखाई दे जाती है। निराकृत आकाश में जिस तरह मेघाकृति पैदा होती, बदलती और विलीन होती दिखाई देती है, उसी तरह निराकार ब्रह्म में राम का सगुण रूप गढ़ा हुआ दिखाई देता है। माता कौशिल्या के वात्सल्य भाव में, भगवान शिव के ज्ञान भाव में, तपःपूत ऋषि-मुनियों के भक्ति-भाव में उन-उन भावों के अनुकूल ब्रह्म-स्वरूप निखरता है। चूँकि राम का प्रकट रूप एक आदर्श नीति-पुरुष का है, सामान्य मनुष्य भी उसमें अपने लोक-जीवन के मूल्यों को चरितार्थ होता देखता है। दूसरी ओर, कृष्ण चरित चूँकि लीलामय है, उसकी बोधगम्यता के लिए भक्ति के तगड़े खुराक की जरुरत होती है। मानुषी कर्म-विधान और ज्ञानलोक के प्रतिमान उसकी समझ तक पहुँच पाने में असमर्थ हैं। जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि है उसे ही वह मिलेंगे। 'भगवद्गीता' में इसीलिए कर्मयोग और ज्ञानयोग अंततः भक्ति योग के अनुषंगी ही सिद्ध होते हैं।
'रामचरित मानस' के राम का मानुषी चरित आध्यात्मिकता का बोध कराने की दृष्टि से अपेक्षया अधिक जटिल है। नीति पुरुष राम के प्रकट मानुषी चरित को उसकी आध्यात्मिक गहराई में 'सत्यं शिवं सुंदरम्' और 'सत्यं ज्ञानमनंतम्' का आकार लेता हुआ देखा जा सकता है इसीलिए कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग समानरुपेण रामपद प्राप्ति के मार्ग हो सकते हैं- (शिवमय) नीतिमत्ता की प्रधानता से कर्मयोग (ज्ञानमय) सत्यव्रतशीलता की प्रधानता से ज्ञानयोग और (सौंदर्यमय) अनंतता की प्रधानता से भक्ति योग। महर्षि मुक्त के अनुसार, तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' में इन तीनों का एक समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। इस तरह रामचरित मानस सरोवर में आध्यात्मिक अवगाहन हेतु चार घाट हैं- ज्ञान घाट, कर्मघाट, भक्तिघाट और महर्षि मुक्त के शब्दों में स्वयं तुलसीदास का गोघाट जो सीधा और सपाट होने से सभी जीवधारियों के लिए अपंग और अपाहिजों के लिए भी सुगम है।
अध्यात्म की दृष्टि से ज्ञान का एक ही अर्थ है - आत्म दर्शन। संसार का ज्ञान विषय-दर्शन है और इसके वाहक हैं इंद्रियां और मन। मन में इच्छा-वासना की निरंतर उठने वाली तरंगें इंद्रियों को विषय-प्रवृत्त करती हैं और रागी-भोगी मनुष्य संसार-सागर में डूबने-उतराने लगता है। विषयभोगाविष्ट यह बोध आत्म दर्शन से उतना ही दूर है जितना अंधकार प्रकाश से। इसलिए वस्तुतः यह ज्ञान की अवस्था न होकर अज्ञान की अवस्था है। साधारणतः आत्मा के निज-रूप पर अज्ञान का यह धुंध छाया रहता है और इसलिए प्रायः मनुष्य आत्म-प्रकाश से वंचित रह जाता है। दूसरी ओर जब आत्म दर्शनपूर्वक व्यक्ति आत्मा को उसके निज रूप में जान लेता है तब उसके लिए संसार का स्वरूप ही जगदाधार आत्मा का, श्रीराम का विमलयश बनकर प्रकाशित होने लगता है। आत्म-ज्ञान के बिना जगत् प्रपंच के आधार तक नहीं पहुँचा जा सकता। इस तरह आत्म-ज्ञान के बिना जगत का भासना ही अज्ञान है। शिवजी को यह ज्ञान है इसीलिए वे श्रीराम के माया-मानुषी चरित से न तो व्यथित होते हैं और न ही हर्षित जबकि माता पार्वती मोहवश संशयग्रस्त हो जाती हैं। आत्म- ज्ञान की स्थिति में जगदाभास रुपी सारे विकल्प जाति-वर्ण, सगुण निर्गुण, गति- स्थिति, परिवर्तन-परावर्तन, देश-काल आदि-आत्मा में ही समा जाते हैं। इस दृष्टि से आत्मा-परमात्मा, व्यष्टि-समष्टि न भेद भी एकांतिक नहीं है। अस्तित्व रूपों के आधार में स्थित जो आत्मा है वही सत्ता मात्र का आधार स्वरुप सर्वात्मा परमात्मा है। शुद्ध सत्ता स्वरूप आत्मा ही परमात्मा श्रीराम हैं, जबकि यह वह अस्तित्व रुपों में जो प्रकट हो रहा है वह 'मैं' आत्मा हूँ।
कर्मघाट में मानस-अवगाहन जगत्-भ्रम या संशयावस्था से छुटकारा पाने का एक अचूक उपाय है। ज्ञान एक उपाय या साधन न होकर उपलब्धि है जबकि कर्म स्वरुपतः एक साधन है, सुख-दुःख प्राप्ति का या रामपद प्राप्ति का भी। श्रीराम का मानुषी चरित प्रकटतः एक कर्म-क्षेत्र है, जहाँ स्त्री-पुरुष विधि-निषेध, राग-विराग आदि सांसारिक विक्षेप पाये जाते हैं। किन्तु जिस क्षण यह बोध होता है कि ये सारे विक्षेप मायावी संरचनाएं हैं, भ्रम मिट जाता है तथा कर्मों और संलग्न भावों का अत्यंताभाव पैदा होता है। तब न कर्ता-भाव रहता है न भोक्ता भाव, न अहंकार, न मोह, न पाप और न पुण्य। जिसे हम 'धर्म' कहते हैं उसका आशय ठीक यही है-न तो उसे करने में लज्जा होती है और न ही भय। इसीलिए धर्म भगवदावतार द्वारा रक्षणीय बनता है। इसके विपरीत जिस कर्म को करने में लज्जा या भय हो, वही अधर्म है। धर्म करने से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में वैराग्य जागता है और वैराग्यवान को ही भगवान को जानने की जिज्ञासा होती है। ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति ने परमानंद पाने की योग्यता हासिल कर ली है। परमानंद से आशय है सुख-दुःख रहित आनंद, ब्रह्मानंद। श्रीराम के इस नित्य स्वरुपानंद का ही वर्णन तुलसीदास के शब्दों में है- 'शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं' जिसमें डूबकर मन कामादि दोष रहित हो जाता है। मन के कामादि दोषवश विषय-मूलक कमों से प्राप्त सुख मनुष्य को अंततः दुःख की ओर ढकेलता है जबकि जन्म-जन्मांतरों में उसकी खोज ऐसे सुख के लिए होती है जिससे दुःख की डोर न बंधी हो। उसकी यह खोज कर्म और कर्मफल से परे उनके आधार में स्थित आत्मा से समस्वरुपता प्राप्त कर लेने पर ही पूरी होती है। तब वह कर्त्ता-भोक्ता, कर्म-क्रिया, सुख-दुःख जैसे द्वंदमूल भावों से पृथक अस्तित्व मात्र के मूलाधार आत्मा के प्रति 'निर्भरा' भाव से समर्पित हो जाता है। यही कर्म संदर्भ में भगवद्वद प्राप्ति के लिए आवश्यक निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म का रहस्य है।
भक्ति घाट में मानस-अवगाहन हेतु उक्त 'निर्भरा' भाव के अतिरिक्त विमल 'प्रेम भाव' की जरुरत होती है। ईश्वर तक पहुँचने के लिए यह सीधा और सरल मार्ग है। यह एक साधन है और उपलब्धि भी। साधना की दृष्टि से भक्ति एक साधन है जबकि वही प्रेममय प्रपत्ति की दृष्टि से एक उपलब्धि है। श्रीकृष्ण के इन शब्दों में भक्ति के दोनों लक्षण विद्यमान हैं- 'सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।' 'परित्याग' में साधना है, जबकि 'शरणागति' उपलब्धि है। रामकथा के प्रसंग में शरणागति की अवस्था प्रेमानंद से परिपूर्ण है। वस्तुतः 'रम्' धातु से निष्पन्न 'राम' शब्द का गूढाशय ही यही है। श्रीराम आनंद रस से परिपूर्ण सागर हैं जिसमें प्रेमीजन सहज ही तैर सकते हैं। शिवजी और काकभुशुण्डी जी के श्रीराम के बाल स्वरूप में रम्यमान होने का रहस्य अब समझ में आ सकता है- बाल रूप सहज भावेन आनंद स्वरूप है, मनसा-वाचा-कर्मणा से परे वह स्वभावसिद्ध है। परमानंद या आत्मानंद की भी यही सहज अवस्था है और इसके प्रति पूर्ण समर्पण का नाम है भक्ति। ऐसी पूर्णतः सहज भक्ति के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कर्म- अकर्म, ज्ञान-अज्ञान, साधन-साध्य बेमानी है। यह तो सर्वत्र व्याप्त आत्म-स्वरुप शुद्ध सत्ता की ही आत्मीय उपलब्धि है। आत्म स्वरुपता ही आत्मानंद है। मेरा अपनी आत्मा से, जीव का उसमें विराज रहे भगवान आत्मा का मिलन केवल सहज, निरावलंब ही हो सकता है। यह आध्यात्मिक 'तल्लीनता' की स्थिति है जिसमें भगवद् भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भाव के लिए जगह बच ही नहीं रह सकती।
प्रकट ही अब तक उल्लिखित मानस के सभी तीन घाट- ज्ञान, भक्ति, कर्म, यत्नवान मानुषी संदर्भ वाले हैं, क्योंकि मानव चेतना में ये पृथक-पृथक रुपेण- व्याकृत हैं। किंतु कण-कण में व्याप्त रहे भगवान और भगवद् प्रसाद के लिए यह विशेष संदर्भ कोई सीमा रेखा नहीं हो सकती। जीवों सहित सारी जड़ प्रकृति के करतब भी तो अपने आधार से, सर्वात्मा से अभिन्नता के लिए ही तो हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास का चौथा घाट-गोघाट, जिसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति का अपृथक्कृत समन्वित भाव है-सबके लिए सुगम एक खुला घाट है। इसमें अवगाहन हेतु पशु- पक्षी, सक्षम-अक्षम, अधिकारी-अनधिकृत, जड-चेतन सभी उतर सकते हैं। सांख्य मतानुसार प्रकृति का सारा खेल पुरुष की मुक्ति के लिए है और इस मुक्ति में अपना लक्ष्य साध कर स्वयं प्रकृति भी मुक्त हो जाती है। वेदांत इसीलिए इस प्रकृति को परम पुरुष की शक्ति रूपी माया कहता है। माया मनुष्य को आईना दिखाती है। यह आईना आत्म-दर्शन के लिए भी है और मोहमूल जगत्-दर्शन के लिए भी। इस माया-जन्य आईने को मनुष्य अपने 'मन' के रूप में पहचानता है। जिसे हम बहु आयामी संसार कहते हैं, वह वस्तुतः द्वि-आयामी मन की सृष्टि है। मन के रागानुरायी सुख और द्वेषानुशयी दुःख ये दो ही आयाम हैं जिनके सहारे वह बहु-आयामी संसार की सृष्टि करता है। हमारा सारा संसार राग-द्वेषमय या मोहमूल है। मन के इस स्वरूप को पहचान लेना ही 'ज्ञान' है और मन को इस तरह जानने वाला 'मैं' आत्मा हूँ। इस तरह आत्मवत् हो जाने से मन की भ्रामक सृष्टि मन सहित 'मैं' में लीन हो जाती है। पाप-पुण्य, कर्म-अकर्म, ज्ञान-अज्ञान आदि सारे द्वैत पिघल कर 'मैं' रुपी अद्वैत में समा जाते हैं। आत्म-दर्शन इसी अद्वैत बोध का नाम है।
परंतु यह भी सच है कि वास्तव में ऐसा आत्म-बोध सहजतः लभ्य नहीं है। इसे सुलभ बनाने के लिए हमें पहले 'कर्म' के रहस्य को समझना होगा। रामकथा प्रसंग में श्रीराम के कष्टमय वनवासी जीवन के लिए निषाद राज माता कैकेयी को दोषी मानते हैं। लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं कि जीव के सुख-दुःख तो स्वयं उसके अपने कर्मों से उपजते हैं और कर्म-जन्य सुख-दुःख को केवल आत्म-दर्शन के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है मन द्वारा बुना हुआ भ्रम जाल, जो हमें विषय-जगत में कर्मों की डोर से बांध कर रखता है। आत्म-दर्शन के लिए मन के इस जाल को शिथिल करना होगा, मन की चंचलता को रोक कर उसे स्थिर करना होगा। इसके लिए उपाय है- अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मन को रोकने का उपाय न होकर, केवल अ-मन होकर रहना है। अ-मन होना अर्थात् चेतना का सहज हो जाना, जैसे जब हम अहं - भाव अथवा व्यष्टि भाव की सजगता के बगैर देखने-सुनने-गुनने की क्रिया करते हैं। दूसरी ओर जब भी हम अपने को कुछ-कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता आदि मान लेते हैं, मन सामने आ खड़ा होता है। बल्कि मान लेना, मान्यता ही मन है जबकि अपने को कुछ भी न मान कर आत्मवत् हो रहना ही अ-मन होना है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है-चूँकि मेरा मानना ही, मान्यता ही मन है, मन का स्वामी 'मैं' आत्मा हूँ अर्थात् मन मेरे वश में हुआ। इसलिए वास्तव में मनस जन्य कर्मों से 'मैं' बंधा हुआ नहीं हूँ, कर्म करते हुए भी 'मैं' अकर्त्ता हूँ। अब मेरी गति मनरचित संसार में न होकर आत्मा के अनंताकाश में है। संसार में इसी गतिहीनता का नाम विराग या वैराग्य है, जिसके बिना ज्ञान संभव नहीं।
द्रष्टव्य है कि 'मैं' के अ-कर्त्ता भाव का एक निषेधमूलक पक्ष है और दूसरा विधानमूलक। संसार से उपरति, अपर वैराग्य, उसका निषेधमूलक पक्ष है और यह सर्वथा संभव है कि मन के विषय-विकल्पों से भरी दुनियाँ में परिस्थिति विशेष में अ-कर्त्ता बना मनुष्य परिस्थिति बदल जाने पर पुनः कर्म की राह पकड ले। अतः जब तक हम उक्त अ-कर्त्ता भाव को ज्ञान की भूमि पर आत्म-दर्शन के आधार पर स्थिर नहीं कर देते, उसकी स्थिति डांवाडोल रह सकती है। दूसरी ओर अ-कर्ता भाव की उक्त तरह की स्थिरता ही पर-वैराग्य है अर्थात् वैराग्य का आत्मदर्शी रूप, • जहाँ से लौटकर मनुष्य पुनः कर्म में, कर्त्ता भाव में लिप्त नहीं होता। यह राग-द्वेष, सुख-दुख से परे आत्मानंद की अवस्था है जिसमें जीव और ब्रह्म का, रामभक्त और राम का भेद समाप्त हो जाता है। शुद्ध भक्ति ईश्वर में प्रेममय प्रपत्ति-पूर्वक अपने पृथक अस्तित्व को भेदमूलक सारे प्रकल्पों को समाप्त कर देने का ही भाव है। परमार्थ तत्वतः अभेद-सिद्धि है।
महर्षि मुक्त के 'रामदर्शन' का यही सार है। वास्तव में 'रामदर्शन' आत्म दर्शन है। वेदांत दर्शन का यही सार-कथ्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग मूलतः प्रभु संयोग में एकीकृत हो जाते हैं। उनमें अभेद-दर्शन ही राम दर्शन है क्योंकि 'राम' स्वरुप में वे अभेदवत् ही प्रकट होते हैं। सत्, चित् और आनंद के पृथक्कृत मानुषी भाव ब्रह्म स्वरुप में एकीकृत 'सच्चिदानंद' बनकर प्रकट होते हैं। 'रामचरित मानस' के राम का माया-मानुषी सगुणचरित अब देश-काल की परिधि से बाहर शाश्वत, सर्वव्यापी, सर्वग्राही चैतन्य तत्व बनकर अपने निर्मल, शुद्ध, निराकृत-निर्गुण रूप में स्थिर हो जाता है। निराकृत निर्गुण राम का यह प्राकट्य ही आत्म दर्शन है। ऐसा आत्म दर्शन ही सगुण राम को समयानुकूल गढ़ता और पूजा प्रतिष्ठा के लिए प्रस्तुत करता है।
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
पूर्व प्राध्यापक दर्शन एवं धर्म विभाग
विश्वभारती विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन (प.वं.)
एवम्
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
उद्गार
मेरे ही स्वात्मस्वरूप
महामहिम -
आपकी महती आकांक्षा का समुचित सम्मान करते हुए "महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति' द्वारा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, राम दर्शन आपको समर्पित किया जा रहा है।
श्री रामचरितमानसान्तर्गत अधिकांशतः जितने भी तत्त्व-परक आध्यात्मिक प्रसंग हैं, यथा-शिव गीता, लक्ष्मण गीता, राम गीता, जनक स्तुति, वाल्मीकि स्तुति, वेद स्तुति, चित्रकूट के चारों दरबार, विभीषणशरणागति, ज्ञान-वैराग्य निरूपण, वंदना एवं राम नाम महिमा आदि के क्लिष्ट भावों का सहज एवं सरल भाष्य, इस पुस्तक की विषय वस्तु है।
राम दर्शन में प्रतिपादित तत्त्व- "प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना" - न सगुण ब्रह्म है और न निर्गुण ब्रह्म, अपितु सगुण-निर्गुण से परे, सगुण-निर्गुण का आधार, सगुण-निर्गुण का द्रष्टा, ज्ञाता, अनुभव से परे है और इसे ही सत्ता, भूमा या अस्तित्व कहते हैं।
जिस अनुभूति में, जिस अनुभूति करके, जिस अनुभूति से परानुभूति की अनुभूति नहीं होती, वही अनुभूति अपना स्वरूप (राम) है।
यह रहस्य कृपा साध्य है और संत शरण के भिखारी हुए बिना इस अनुभूति की अनुभूति होना सम्भव नहीं है।
समझेगा वही सुह्वत पसंद बन गया दोस्त दरवेशों का ।
ये दिल दिमाग की चीज नहीं जो करता है सो खो बैठा ।।
श्रीरामचरितमानस की सभी चौपाइयाँ मंत्र हैं और प्रस्तुत पुस्तक रामदर्शन इन मंत्रों का भाष्य है। इस तरह का भाष्य वही कर सकता है, जिनके पास अनुभव बल हो, आत्मबल हो, आत्म निष्ठा हो, गुरुओं की महान कृपा हो और विद्वान भी हो, तब ही इस तरह का विवेचन हो सकता है, यह भगवान की देन है, खाली विद्वत्ता नहीं।
महर्षि मुक्त द्वारा समय-समय पर हुए श्री रामचरित मानस के आधार पर आध्यात्मिक प्रवचनों के इस संकलन को मूर्त रूप दिया है, स्व. श्री झुम्मुकलाल जी दीन, दुर्ग ने।
समिति श्री दीन जी का आभारी है, जिन्होंने महर्षि मुक्त के सान्निध्य में रहकर उनकी अनुमति से ही उनकी अनुभूतियों को शब्दों में पिरोकर जन कल्याणार्थ प्रकाशित कर, उन्हीं के चरणों में समर्पित कर, इस उक्ति को चरितार्थ किया।
मेरा कुछ भी है नहीं, जो कुछ है सो तोर ।
तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर ।।
उसी पूर्व प्रकाशित पुस्तक का यह नव-संस्करण, नवीन परिधान से वेष्टित कर आपके कल्याणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले यह तीन खण्डों में था, अब तीन भागों को एक में सम्मिलित करके इसे रामदर्शन (सम्पूर्ण) नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं।
रामदर्शन (सम्पूर्ण) श्री रामचरित मानस प्रेमियों के लिए वरदान सिद्ध हुई है, इसीलिए इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पुनः प्रकाशन का निर्णय लिया गया।
रामदर्शन का श्रद्धापूर्वक पठन, मनन, निदिध्यासन से रामदर्शन में किञ्चित संदेह नहीं, इसके ठीक विपरीत -
अगरचे कुतुब अपनी जगह से टले तो टल जाये ।
बहर जुगनू की दुम से जले तो जल जाये ।
हिमालय बाद की ठोकर से गो फिसल जाये ।
और आफताब भी किबले-उरूज ढल जाये ।।
यद्यपि ये सम्भव नहीं फिर भी ऐसा हो जाये। मगर मंदमति, विषयासक्त, दुराग्रही और कुतर्की जैसे प्रपञ्ची दरिद्र जीवों के लिए इसका भाव, ग्रहण करना असम्भव है, इसलिए रामदर्शन (सम्पूर्ण) "दनुज विमोहन, जन सुखकारी" है।
यह विश्व में अपनी शानी का एक ही साहित्य है। प्रमाण? हाथ कंगन को आरसी क्या। बकौल महर्षि मुक्त -
मस्ती में मस्त होकर मस्ती को लिख रहा हूँ।
मस्ती में मस्त पढ़ना दरिया नजर आयेगा ।।
यूँ तो शुद्धाशुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसमें श्री नारद दुबेले और श्रीराम प्रसाद साहू का प्रयास प्रशंसनीय है, फिर भी कहीं-कहीं पर यदि अशुद्धि रह गयी हो तो सुधि-जन इसे सुधारकर पढ़ें और समिति को क्षमा करें। क्योंकि
अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना ।
गब्बस को मतलब है सदफ से या गौहर से ।।
अलम् !
अध्यक्ष
(डॉ. सत्यानन्द त्रिपाठी)
महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक
समिति
आरती
आरती सद्गुरुदेव नमामी । पार ब्रह्म-प्रभु अन्तर्यामी ।
अगुण अपार अलख अविनाशी । अचल विमल प्रभु सब उर वासी ॥
निर्गुण निर्विकार सुखरासी । एक अरूप अलेख अनामी ।।1।।
महिमा नेति नेति श्रुति गावें । नित्य निरंजन सब बतलावें ।॥
शेष शारदा पार न पावें । जय सच्चिदानंद अभिरामी ।।2।।
वचन किरण तम मोह विनाशक । ज्ञान सूर्य माया के शासक ॥
दिव्य दृष्टि के परम प्रकाशक । ब्रह्मादिक सुर सेव्य नमामी ॥३॥
जब तक कृपा न तुम प्रभु करते। विधि हरिहर क्या भव से तरते ॥
असविचारि गुरु भक्ति जो करते। मिलते राम उन्हें सुखधामी ॥4॥
गुरुवर चरण कमल की छाया । करती दूर ताप त्रय माया ||
जब तक पूर्ण न होवे दाया । मिलत नहीं शिव अन्तर्यामी ॥5॥
भक्ति ज्ञान वैराग्य नियम के । रूप सकल इंद्रिय संयम के ।
भूषण शम दम पंच सुयम के । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मम स्वामी ॥6॥
जीवन धन मंजुल निज जन के । अंकुश मद मतंग जन मन के ॥
शुचि पथ परमारथ पथिकन के। इक रस आनंद रूप नमामी |17||
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
॥ बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय ॥
महर्षि मुक्त
महर्षि मुक्त जैसे थे वैसे ही थे। यदि कोई यह दावा करे कि ऐसे थे और वैसे थे, तो उनका दावा गलत ही होगा। अपने परिचय में वे स्वयं कहा करते थे - " हैं तो हम अजन्मा" लेकिन हमें आप लोगों के खातिर आना पड़ा।"
उन्होंने यह भी कहा था भगवान को तो जान सकते हो क्योंकि वह तुम्हारा आत्मा है, परन्तु मुक्त को समझना बहुत ही कठिन (असम्भव) है।' आत्मा का लक्षण होता है परन्तु इनका तो कोई लक्षण ही नहीं था। ऐसे अलक्षण को यदि कोई जान जाय तो बन्ध्या का पुत्र सिंह का शिकार कर सकता है।
अपने पचास वर्षों के अनवरत प्रचार में जिस सिद्धांत या धर्म की इन्होंने प्रतिष्ठा की उस धर्म को महात्मा करपात्री जी ने 'ज़िंदा वेदान्त' (अनुभवयुक्त ) कहा है और यह भी कहा उन्होने कि - "अभी विश्व में जिंदा वेदान्त (सत्य धर्म) का प्रचार कोई कर रहे हैं तो महर्षि मुक्त ही हैं।"
शास्त्रों ने इनका परिचय इस प्रकार दिया है -
यस्यान्तं नादि मध्यं नहि कर चरणं नाम गोत्रं न सूत्रम्,
नो जातिर्नैव वर्णाः नहि भवति पुरूषो न नपुंसो न च स्त्री।
नाकारं नैवकारं नहि जनि मरणं नास्ति पुण्यं न पापम्,
तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहज समरसं ।
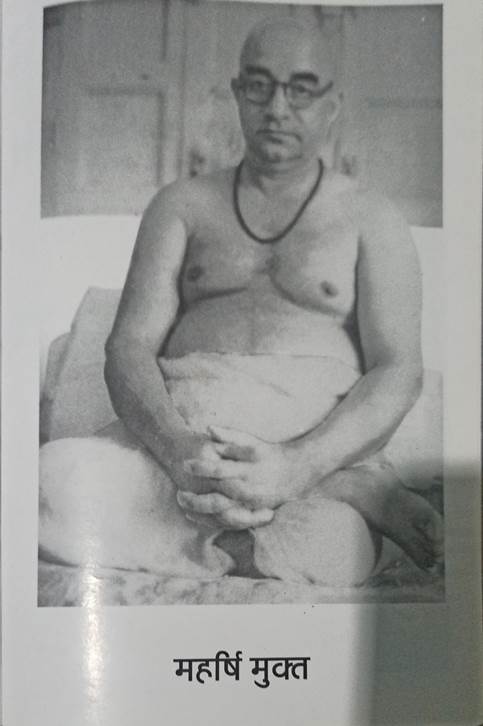
विषय-सूची
तृतीयावृत्ति पर संक्षिप्त उद्बोधन
7. भगवान शंकर और माता पार्वती सम्वाद
प्रथम खण्ड़
1. शिव गीता
2. राम नाम महिमा
3. मनु शतरुपा वरदान
।। श्री गणेशाय नमः ।।
।। श्री गुरुवे नमः ।।
1. शिवगीता
नारायणोपनिषत्
ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति। नारायणात्प्राणो जायते। मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणाद् ब्रह्मा जायते। नारायणाद् रुद्रो जायते। नारायणाद् इन्द्रो जायते। नारायणात्प्रजापतिः प्रजायते।
नारायणाद्वादशाऽऽदित्याः सर्वे रुद्रा सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणिछन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात्प्रवर्तन्ते। नारायणे प्रलीयन्ते।
अथ नित्यो नारायणः। ब्रह्मा नारायणः। शिवश्च नारायणः। शक्रश्च नारायणः। कालश्च नारायणः। दिशश्च नारायणः विदिश्च नारायणः। ऊर्ध्वच नारायणः। अधश्च नारायणः। अन्तर्बहिश्च नारायणः।
नारायण एवेदंसर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् निष्कलङ्को निरञ्जनो, निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति।।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
रामाय राम भद्राय, रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय, सीतायाः पतये नमः यन्मायावशवर्त्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भमः।। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां । वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।।
अनन्त नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्वेन प्रस्फुरित, महामहिम, स्वात्मस्वरूप सकल चराचर वृन्द एवं समुपस्थित आत्म जिज्ञासु गण। 'उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत्।'
अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवो। उठो। स्व- स्वरूप भगवान आत्मा में जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर अपना आत्म कल्याण करो। मानव जीवन का यही चरम लक्ष्य है।
यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवचन श्री रामचरित मानस के आधार पर हो रहा है। रामचरित मानस (रामायण) भारत वर्ष की अनुपम विभूति है। यह संसार के कोने- कोने में फैला हुआ है। विदेशों में भी इसका प्रचार है। रामायण में क्या नहीं है, इसम ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, राजनीति, धर्मनीति आदि सभी कुछ भरा पड़ा है। रामायण की भाषा, अत्यन्त सरल, सरस, रोचक और भावपूर्ण है। इसके भाव सभी के समझ में आने लायक है। इसका महत्व केवल इस देश में ही नहीं, सर्वत्र इसकी प्रतिभा की छटा छिटकी पड़ रही है। हिन्दी जगत् में ऐसा ग्रन्थ न बना है और न भविष्य में इस तरह की आशा है। इसमें चारों वेद, छः हों शास्त्र, उपनिषद्, श्रुति, स्मृति आदि सभी का समन्वय है।
व्यवहार जगत् में पिता के प्रति पुत्र का, पुत्र के प्रति पिता का, भाई के प्रति भाई का, स्त्री के प्रति पुरुष का, पुरुष के प्रति स्त्री का, गुरु के प्रति शिष्य का, शिष्य के प्रति गुरु का, राजा के प्रति प्रजा का, प्रजा के प्रति राजा का, स्वामी के प्रति सेवक का, सेवक के प्रति स्वामी का, क्या कर्त्तव्य है? रामायण में यह सब मिलेगा। प्रत्येक की मर्यादा का यहाँ उल्लेख है। यह एक अलौकिक ग्रन्थ है।
बोधवान होकर व्यवहारिक जगत् में, व्यवहार कैसे करना है, यह रामायण सिखाती है।
जिस देशमें ईश्वर और धर्म के प्रति स्थान नहीं है, उस देश में भी राजनैतिक दृष्टिकोण से लोग इसे अपनाते हैं।
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा ।
भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ।।
अर्थात् मैंने (तुलसीदास ने) अपने अन्तःकरण के सुख के लिए इसकी रचना की। तब यहाँ पर शंका होती है कि क्या गोसाई जी महाराज बड़े स्वार्थी थे?
नहीं! इसका दूसरा अर्थ -
"शुष्ठ अन्तःकरण", याने स्वान्तःकरण अर्थात् जिनके सुन्दर पवित्र अन्तःकरण हैं, उनके लिए इस ग्रन्थ की रचना की गयी, जिससे "मतिमञ्जुलमातनोति" उनकी कोमल बुद्धि प्रसारित हो। हृदय मोम बने।
"स्वान्तः सुखाय" जिनके शुष्क हृदय हैं, उन्हें हरा-भरा करने के लिए, श्रुतियों, स्मृतियों, वेदों तथा शास्त्रों सभी का निचोड इस ग्रन्थ में भरा गया।
वेदों की रचना ब्रह्मा ने नहीं की, यह तो ब्रह्मा के मुख से निकले, इसी प्रकार रामायण की रचना, तुलसीदास ने नहीं किया, इसकी रचना तो शिवजी के द्वारा पहिले से ही की गई थी और उन्होंने इसे अपने मन में रखा था, जिसको सुन्दर समय पाकर उन्होंने माता पार्वती को सुनायी। इसलिए इस ग्रन्थ का नाम "रामचरितमानस'" पड़ा, जो तुलसीदास जी के मुख से निकला है।
रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ।।
तातें रामचरितमानस बर। घरेउ नाम हियें हेरि हरषि हर ।।
भैय्या। रामचरितमान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है।
भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।
याभ्यां बिना न पश्यन्ति, सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् ।।
माता पार्वती श्रद्धा रूप और भगवान शंकर विश्वास रूप हैं, क्योंकि सारे चराचर का अस्तित्व, विश्वात्मा भगवान राम (ईश्वर) 'मैं' आत्मा रूप में, रग-रग में व्यापक है। फिर भी उसे बिना श्रद्धा और विश्वास के देख नहीं सकते। मानसकार कहते हैं -
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् ।
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ।।
अर्थात् नित्य बोधस्वरूप गुरु अहं वन्दे, शंकर रूप गुरु की मैं वन्दना करता हूँ, क्योंकि नित्य ज्ञान-स्वरूप गुरु की उपमा भगवान शंकर से दी गयी।
जैसे, द्वितीया का चन्द्रमा यद्यपि हँसिया के समान टेढा होता है। परन्तु, फिर भी भगवान् शंकर के मस्तक में रहने के कारण उनके आश्रित होने से संसार उसकी वन्दना करता है, इसी प्रकार यह रचना, यद्यपि टेढी-मेढी है, फिर भी नित्य बोधस्वरूप भगवान शंकर के आश्रित होने के कारण जगत वन्दनीय है।
धार्मिक तत्त्व के पर्वत से अभिभूषित रम्य मनोहर है ।
राम की भक्ति अहै इसमें, भरपूर भरा जल सुन्दर है ।।
मौक्तिक हैं मिलते उपदेश, अलभ्य महा सुख निर्झर है ।
प्रेमी मराल गणों के लिए, यह मानस मान सरोवर है ।।
तुलसीकृत राम कथा जग में, नर नारिन तारन को पुल सी ।
पुलसी भव सागर पारन को, पढ़के मन गाँठ गई खुल सी ।
खुलसी गई पापन की गठरी, घुल सी गई जनता अरु हुलसी ।
हुलसी जनता, हुलसी वसुधा, हुलसी-हुलसी, जन के हुलसी ।।
एक बार हनुमान जी ने पहाड़ पर अपने नाखून से पत्थर गढ़-गढ़ कर सातो काण्ड रामायण लिखा और वे उस पहाड़ को भगवान राम के पास ले जाकर विनीत भाव से बोले- "भगवन! मैं सरकारी चरित्र लिख कर लाया हूँ, आप इसे देखकर इसमें अपना हस्ताक्षर कर दीजिये।"
भगवान राम ने उसे ध्यान से देखा तथा पढकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हनुमान जी तुमने बहुत परिश्रम किया है। भैया, तुम्हारा यह परिश्रम प्रशंसनीय है। परन्तु, देखो अभी-अभी श्री वाल्मीकि जी भी एक रामायण लिखकर ले आये थे। मैंने उसमें अपने हस्ताक्षर कर दिए है। अब तुम इसे मेरी आज्ञा से उनके पास ले जाओ और उनसे अपने हस्ताक्षर करने के लिए कहना, यदि वे अपना हस्ताक्षकर कर देते हैं तो उसे मेरा हस्ताक्षर समझना।
भगवान राम की आज्ञानुसार हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर श्री वाल्मीकि जी के पास ले गये, वाल्मीकि जी उस समय किसी समुद्र के किनारे रहते थे। श्री हनुमान जी ने उन्हें रामाज्ञा सुनाकर उसमें हस्ताक्षर करने को कहा। वाल्मीकि जी ने उसे इधर-उधर से देखा और उपेक्षा की भावना से यह कहकर इसमें सब बातें स्पष्ट नहीं लिखी गयी हैं, इसमें गोसा पर्दा (लुका-छिपी की बातें) है। उसे समुद्र में फेंक दिये। इस पर हनुमान जी बड़े दुःखी और क्रोधित हुए। वे क्रोध में भरकर बोले- देखो, मैं इतने परिश्रम और श्रद्धा से सरकारी चरित्र लिखकर भगवान के पास ले गया। उन्होंने आपके पास भेजा, परन्तु आपने मेरे परिश्रम की उपेक्षा करते हुए तुच्छ समझकर अभिमानपूर्वक उसे समुद्र में फेंक दिया। आपको अपनी कविता का इतना अभिमान है। अब मैं आपको श्राप देता हूँ कि यद्यपि ब्रह्मनिष्ठ का पुनर्जन्म नही होता, परन्तु फिर भी आपको जन्म लेना पड़ेगा और आपने जिस रामायण को उपेक्षापूर्वक समुद्र में फेंका है, उसी को अपने ही हाथों से लिखना पड़ेगा। वाल्मीकि जी भी कम नहीं थे, उन्होंने भी हनुमान जी को श्राप देने के लिए कमण्डल से जल उठाया। हनुमानजी तुरन्त समझ गये और वे उनके चरणों में गिर कर नम्र भाव से कहने लगे - "भगवन्! ऐसा मत कीजिए। इसमें आपके द्वारा सारे विश्व का कल्याण होना है। कलियुग के जीवों के उद्धार के लिए आप निमित्त होंगे। अतः, क्षमा कीजिए और संसार के जन कल्याण के लिए मेरा अभिशाप स्वीकार कीजिए। इस रामायण को लिखते समय जहाँ कहीं पर आप भूलेंगे, मैं समय-समय पर आकर आपकी सहायता करूँगा।" इस पर वाल्मीकि जी शान्त हो गये। भैय्या ! यह गोपनीय रहस्य है। बड़े-बड़े महात्माओं के द्वारा तथा हमने स्वयं कुछ काल एकान्तवास करके इसका अध्ययन किया है, यह कहीं नहीं लिखा है। इस तरह वाल्मीकि जी ही तुलसीदास हुए और इस रामायण को लिखे।
कलि कुटिल जीव निस्तार हित. वाल्मीकि तुलसी भये ।।
वाल्मीकि जी ने जो कहा था कि इसमें बातें साफ-साफ नहीं लिखी गयी हैं, लुका-छिपी की गयी है, वह यह है कि इन्द्र के पुत्र जयन्त के संबंध में जब सीताजी के लिए "सीता चरन चोंच हति भागा" लिखा है। इसको वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि जयन्त ने सीताजी के स्तन में चोंच मारा। अब तुलसीदास जी भी चोंच मारना, लिख तो वही रहे हैं, परन्तु कहाँ पर मारा यह नहीं बता रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि -
"सीता चरन चोंच हति भागा" अर्थात् जयन्त ने सीता जी को अपने चरण से अर्थात् पंजों से और चोंच से आहत किया, मारा। चरण और चोंच दोनों से मारा, पर कहाँ पर? यह नहीं बताया। अपने शब्दों में नहीं कहा, पर भाव स्तन पर मारने का ही रखा, क्योंकि जिस समय चोंच और चरण मारा, उस समय भगवान राम, माता सीता जी के जंघे पर सिर रखकर लेटे हुए थे। इस परिस्थिति में जयन्त यदि सीताजी के चरण में चोंच मारता तो वह भगवान राम को कैसे पता चलता? क्योंकि पैर से खून बहता, तो वह नीचे की ही ओर जाता, जिसे भगवान राम लेटे-लेटे नहीं जान सकते। स्तन में ही चोंच मारने पर खून बहने पर वे तुरन्त लेटे-लेटे ही जान गये-
"चला रुधिर रघुनायक जाना ।"
चोंच स्तन में ही मारा गया तभी तो भगवान बिना बताये लेटे-लेटे ही जान गये। इस तरह तुलसीदास जी ने चोंच के स्थान को अपने मुँह से व्यक्त नहीं किया, क्योंकि सीता जी के प्रति उनकी माता की दृष्टि थी। अतः, ऐसा कहना मर्यादाविहीन था।
इसी को गोसा पट्टी कहकर, वाल्मीकि जी ने क्रोध किया था और उनके द्वारा लिखी गयी रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। इसी तरह कहीं-कहीं कुछ और प्रसंग है। भैय्या, यह अभूतपूर्व रचना है, इसमें ऐसे-ऐसे मार्मिक स्थल हैं कि बिना महान् पुरुषों की कृपा के लगते नहीं, चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो। रामायण की रचना करते समय, हनुमान जी ने सहायता कहाँ पहुँचायी है, इस प्रसंग पर थोड़ा प्रकाश डाला जा रहा है।
बालकाण्ड में सीता स्वयंवर के समय एक प्रसंग आता है कि -
संकर चापु जहाजु, सागरु रघुबर बाहुबल ।
बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस ।।
सोरठा के तीन चरण की रचना जब तुलसीदास जी ने कर ली, तब वे सोचने लगे कि मैंने शंकर जी के धनुष को, जहाज कहा और भगवान राम की भुजाओं के बल को सागर की उपमा दी, जहाँ कि जहाज तैर रहा है, अब जितने राजे-महाराजे, सन्त- महात्मा, ऋषि-मुनि उस स्वयंवर में उपस्थित हैं, वे सब-
"बूड़ेउ सकल समाज ॥"
लिख डालने पर डूब गये। तब वे सोचने लगे कि यह मैंने क्या लिख दिया। डूबे तो अभिमानी राजे-महाराजे ही, जिनको भगवान राम की भुजाओं के बल का अज्ञान था और जो धनुष को नहीं तोड़ सकने पर लज्जित होकर, अपनी-अपनी जगह पर जा बैठे थे। उनका धनुष तोड़ने के लिए उठना, मानों चाप रूपी जहाज पर चढ़ना है और उसे नहीं तोड़ सकना ही डूब जाना है। तो डूबे तो यही लोग, न कि वहाँ उपस्थित सन्त-महात्मा, ऋषि-मुनि आदि लोग। परन्तु, मैंने "बूड़ेउ सकल समाज" लिखकर सबका डूब जाना लिख डाला और लिखा हुआ काटा नहीं जा सकता, उस पर हरताल नहीं फेरा जा सकता। अब, आगे क्या कहा जाये? इस उलझन को कैसे सुलझाऊँ। बस, इसी चिन्ता में वे बड़ी देर तक सोचते बैठे रहे, जब वे इस कठिनाई को नहीं हल कर सके, तब अन्त में यह सोचकर कि पहिले स्नान कर आवें, फिर शांत चित्त से और ठण्डे दिमाग से इसे सोचेंगे, वे अपना कमण्डल उठाये और गंगा स्नान को चल दिये। वहाँ से लौटकर आने पर निश्चिन्त हो, जब वे फिर लिखने बैठे, तब उस सोरठा को पूरा लिखा पाया। उसका चौथा चरण पूरा हो चुका था। लिखा था-
"चढ़े जो प्रथमहिं मोह बस ।।"
इसका मतलब था, सब नहीं डूबे, वे ही डूबे, जिन्हें भगवान राम की भुजा के बल का अज्ञान था और जो अपनी ताकत आजमाने धनुष तोड़ने उठे थे। अर्थात्, उस जहाज पर बैठे थे। तुलसीदास जी समझ गये कि यह सहायता अर्थात् चौथे चरण की पूर्ति, हनुमान जी द्वारा की गयी है।
यह एक सरोवर है। मानसकार कहते हैं कि तालाब में घाट होते हैं, इस मानसरोवर में चार घाट हैं। कोई भी कथावाचक चार ही घाट में कथा करते हैं- 1. भगवान शंकर और पार्वती, 2. महात्मा कागभुसुण्डी और गरुड़, 3. महर्षि याज्ञवल्क्य और भारद्वाज और 4. गोसाई तुलसीदास और भक्तगण। ये चारों के संवाद ही चार घाट हैं-
सुठि सुन्दर संवाद बर, बिरचे बुद्धि बिचारि ।
तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥
यही इस पवित्र और सुन्दर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। चार घाट के चार नाम हैं- 1. राजघाट (ज्ञान घाट), 2. प्रजा घाट (कर्म घाट), 3. स्त्री घाट (भक्ति घाट), 4. गौ घाट (जहाँ पर सभी विषयों पर समन्वय हो, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सबका मिश्रण)।
इन घाटों में जहाँ कहीं भी ज्ञान का प्रसंग आया है, वह माता पार्वती और भगवान शंकर के प्रसंग में आया है। जहाँ कहीं विधि-निषेध का प्रसंग है, वहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद है। जहाँ कहीं भक्ति का विवेचन हुआ है, वह महात्मा कागभुसुण्डी और गरुड़ के संवाद में है और रामायण में जिस प्रसंग में, ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, वैराग्य भी हो, सभी का समन्वय हो तो समझ लेना कि यह गोस्वामी तुलसीदास जी का गौ घाट है और घाटों में तो सीढियाँ बनी रहती हैं, मगर गौ घाट में कोई सीढ़ी नहीं होती, यह ढालू और सलामीदार होती है, जिसमें कि वहाँ लूले, लँगड़े, अन्धे, अपाहिज, पशु-पक्षी आदि सभी जाकर पानी पी सकें। इसलिए, इस घाट का नाम गौ घाट पड़ा। जैसे, रामायाण का अयोध्याकाण्ड, लक्ष्मण गीता है (लक्ष्मण-निषाद संवाद)।
बोले लखन मधुर मृदु बानी। ग्यान बिराग भगति रस सानी ।। से लेकर
सखा समुझि अस परिहरि मोहू। सिय रघुबीर चरन रत होहू ।। तक।
ऐसे प्रसंग जहाँ पर आवे तो समझ लेना कि यह गोसाई जी का घाट है, इसमें सात सीढ़ियाँ हैं -
सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ग्यान नयन निरखत मनमाना ।।
सातों काण्ड सात सीढ़ियाँ हैं। ज्ञान की सात भूमिका ही सात सीढ़ियाँ हैं। 1. शुभेच्छा, 2. विचारणा, 3. तनुमानसा, 4. सत्वापत्ती, 5. असंसक्ति, 6. पदार्थाभावनी, 7. तुर्यगा।
1. शुभेच्छा (बालकाण्ड) -
शुभेच्छा से भरा पड़ा है। महर्षि भारद्वाज की इच्छा हुई कि मैं भगवान राम की कथा सुनूँ। माता सती की इच्छा हुई, कि मैं रामचरित्र सुनूँ। महाराज दशरथ की इच्छा हुई कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाऊँ। राजा जनक की इच्छा हुई कि सीता स्वयंवर करूँ।
2. विचारणा (अयोध्याकाण्ड) -
श्रवन समीप भये सित केसा, मनहुँ जरठपनु यह उपदेसा ।
इसलिए, श्रीराम को युवराज पद दे देने का विचार हुआ। देवताओं का विचार हुआ कि अगर राम राज्य में फँस गये, तो हम सबों का बड़ा अहित होगा। अतः, सरस्वती को भेजकर मंथरा की बुद्धि पलटने का विचार हुआ। मंथरा का विचार कैकेई को मंत्रणा देने का हुआ। सीता जी और लक्ष्मण का विचार हुआ कि हम भी सरकारी सेवा में राम के साथ वन जायें। महात्मा भरत का विचार हुआ कि "देखें बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनि न जाइ" अयोध्यावासी तथा गुरु वशिष्ठ और जनक का विचार चित्रकूट जाने का हुआ। मतलब यह कि अयोध्याकाण्ड 'विचारणा' भूमिका से भरा पड़ा है।
3. तनुमानसा (अरण्यकाण्ड)
लक्ष्मण के सात प्रश्न-"कहहु ग्यान बिराग अरु माया" माया, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति क्या है और जीव, ईश्वर का भेद क्या है? इस भूमिका में इन सबों का निश्चय हुआ।
4. असंसक्ति (सुन्दरकाण्ड) -
सब कुछ त्यागकर विभीषण भगवान की शरण में आता है -
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ।।
सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ।।
समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहिं मन माहीं ।।
अस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसइ धनु जैसे ।।
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । घरउँ देह नहि आन निहोरे ।।
देखो, अवतार लेने का जो कारण है, उसका पता इस चौपाई से चलता है। अजन्मा भगवान का जन्म क्यों होता है। सर्व त्याग का फल यही हुआ कि विभीषण की सन्त श्रेणी में गणना हो गयी और साथ ही त्रैलोक्य का स्वामी हो गया। यह भगवत् शरणागति का फल है।
6. पदार्थाभावनी (लंकाकाण्ड) -
जगदाकार वृत्ति का लोप होकर ब्रह्माकार वृत्ति का होना।
दोहा-
बिस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन बिस्वासु ।
लोक कल्पना बेद कर। अंग अंग प्रति जासु ।।12 (क) ।।
ऐसा मन्दोदरी ने रावण से कहा है।
7. तुर्यगा -
उत्तरकाण्ड सबसे भरा हुआ है। पूर्ण ज्ञान और भक्ति का उदय इसमें ज्ञान दीपक, सन्त लक्षण, महात्मा कागभुसुण्डी जी की कथा है।
सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मनमाना ।।
भैय्या! जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हों, वही इसका जल पी सकता है। आँख वाला ही इस सरोवर की सीढियों से उतरकर उसमें स्नान कर सकता है, जलपान कर सकता है, अज्ञानी अंधों के वश की बात नहीं है। वे यहाँ नहीं आ सकते। जो प्रसंगानुसार अर्थ करते हैं और समझते हैं, वे ही इस सरोवर के रक्षक हैं।
जिन्होंने सन्त समागम किया है, सन्तों के चरणरज का अपने मस्तक पर अभिषेक किया है, वे ही इसके अधिकारी हैं।
जो विश्वास और श्रद्धा से विहीन हैं, सन्तों का कभी संग नहीं किया है, वे इसके अनधिकारी हैं।
दोहा-
श्रोता वकता ग्याननिधि, कथा राम कै गूढ़ ।
किमि समुझौं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित बिमूढ़ ।।30 ख।।
इसके श्रोता और वक्ता दोनों को ज्ञान निधि होना चाहिए तभी यह समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है, जब तक सत्य वस्तु 'मैं' आत्मा चराचर का अस्तित्व सर्व का 'मैं' को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक श्रीराम चरित मानस को न कोई समझा सकेगा और न कोई समझ सकेगा। सन्तों की कृपा से ही यह समझा जा सकता है। इसलिए -
जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करउ मनलाई ।।
कथावाचक तीन प्रकार के होते हैं -
1. विषय सूची, रुचिर शब्दावली के ही विवेचन करने वाले होते हैं, उनको अमुक शब्द रामायण में कहाँ-कहाँ पर कितनी बार आया है। बस, इसी की रोचक व्याख्या करने और अपनी मिथ्या पाण्डित्य और विद्वत्ता के प्रदर्शन में ही आनन्द आता है। लोग भी समझते हैं कि पण्डितजी कितने महान विद्वान हैं, सारी रामायण इनके करतल गत हैं। इस व्याख्या से न तो श्रोता के पल्ले कुछ पड़ना है और न वक्ता के।
2. इतिहास, लीला भाग के ही कथन करने वाले होते हैं।
3. तत्त्व का विवेचन करने वाले होते हैं।
रामायण का अर्थ होता है-राम, अस्य, अयन अर्थात रामायण, अयन का अर्थ होता है-विश्राम, निवास। इस तरह राम का जो विश्राम स्थल, निवास स्थान है, उसको कहते हैं, रामायण। राम जिसमें व्याप्य हैं, उसको कहते हैं अयन और जो व्यापक है, उसको कहते हैं, राम। दोनों मिलकर हो गया, रामायण।
व्याप्य 'अयन' है, और व्यापक 'राम' हैं। यदि, अयन नहीं होगा तो राम व्यापेगा किसमें और राम नहीं होगा तो अयन किसका होगा? जैसे, इस मकान में कोई नहीं रहेगा तो मकान रहेगा क्या? नहीं और मकान नहीं रहेगा तो रहने वाला कहाँ रहेगा? इसी प्रकार तृण से आदि ब्रह्मा पर्यन्त अयन हैं और उसमें जो व्यापक है, वह राम है। दोनों मिलकर हो गया रामायण।
एक तृण से लेकर ब्रह्मा तक क्या कोई ऐसी वस्तु है, जिसमें 'है' अस्तित्व सामान्य चेतन न हो? 'है' सबमें है। बिना 'है' अस्तित्व के किसी की भी सिद्धि नहीं। 'है' के बिना 'है' नहीं और 'है' के बिना 'नहीं' नहीं। 'हैं' के बिना न 'है' है और न 'नहीं' है। दोनों की सिद्धि 'है' करके ही है। 'है' से कोई देश, काल, वस्तु खाली नहीं है। यही अस्तित्व 'मैं' आत्मा भगवान राम की व्यापकता है। अस्तित्व पर जो आधारित है, वह है अयन। राम का अर्थ होता है-
"यस्मिन रमन्ते योगिनः सः रामः ।''
जिसमें, योगी महात्माजन रमते हैं, रमण करते हैं, मस्त रहते हैं, खेलते- कूदते, खाते-पीते, चलते-फिरते, देखते-सुनते, सोते-जागते और निवास करते हैं, उसे कहते हैं 'राम'।
प्रश्न होता है- किसमें योगी, महात्मा जन रमण करते हैं? उत्तर है- "चराचरे सुभूतेषु रमन्ते, यस्मिन, सः रामः।"
जो सारे चराचर में रम रहे हैं, अस्तित्व, सत्तामात्र है, सत्ता पद है, उसी में योगीजन रमते हैं। किसमें? अरे, जो सारे चराचर में रम रहे हैं, उसमें। जो सारे चराचर में रम रहे हैं, इसका क्या भाव है?
सुन्दरकाण्ड के मंगलाचरण का एक श्लोक है -
नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये ।
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।।
आत्मा कहते हैं, अस्तित्व को। जो अस्तित्व 'मैं' आत्मा 'राम' सारे चराचर में है, वही 'मैं' हूँ। यही 'राम' शब्द का लक्ष्य है। 'रमुक क्रीडायां' धातु से राम शब्द बनता है। जिस चराचर में रमें हैं और जो सारे चराचर में रमे हैं, दोनों को मिलाकर हो गया रामायण।
देखो, इस हार (फूल की माला) में प्रत्येक फूल का आधार है, धागा। अगर इस हार से धागा निकाल लिया जाय, तो हार का अस्तित्व खतम हो जायेगा। हार नहीं रह सकेगा। इसी तरह जिसको तुम संसार कहते हो, उसका आधार 'मैं' आत्मा ही तो हूँ। जिस आधार पर संसार रूप दिखाई दे रहा है। क्या वह 'मैं' से भिन्न है? यदि 'मैं' आत्मा आधार न रहूँ तो संसार किसके आधार पर टिकेगा? यह रहेगा कहाँ? फिर, किसको संसार कहोगे? इसलिए, तृण से लेकर ब्रह्मा तक सर्व का आधार 'मैं' आत्मा ही हूँ।
भैय्या! फिर समझो देखो, यह अटल सिद्धांत है कि जो जिसमें व्यापक होता है, वही उसका आधार होता है। जो जिसका आधार होता है, वही उसका कारण होता है और जो जिसका कारण होता है, वही उसका स्वरूप होता है।
विषय समझो देखो, यह डण्डा है। इस डण्डे में लकडी व्यापक है। इस डण्डे के रग-रग में लकड़ी परिपूर्ण है। डण्डे में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहाँ लकड़ी न हो, इस तरह डण्डे में लकड़ी व्यापक हुई।
डण्डे का लकड़ी आधार है। यदि, इसमें से लकड़ी निकाल लो तो डण्डा रहेगा? नहीं। डण्डे का अस्तित्व खतम। इसलिए डण्डे का आधार लकड़ी है। डण्डे का कारण, लकड़ी है। यदि लकड़ी न होगी तो डण्डा किसको कहोगे? बिना लकड़ी के डण्डा नहीं रह सकता। अतः, लकड़ी डण्डे का कारण है और डण्डा का लकड़ी ही असली स्वरूप है। लकड़ी ही है, जो डण्डा है।
इसी तरह 'है' अस्तित्व सामान्य चेतन (विशेष चेतन 'मैं' आत्मा भगवान राम) सर्व में व्यापक है, सर्व का आधार है, सर्व का कारण है। सर्व का वही रूप ही है। उससे भिन्न एक तृण की भी अलग सत्ता नहीं। सर्व वही है।
राम का अर्थ होता है-देखो 'राम' में दो अक्षर हैं, रा और म। 'रा' का अर्थ होता है-तत्, अर्थात् 'वह' और 'म' का अर्थ होता है-त्वं, अर्थात् तू। अब दोनों अक्षरों को मिला दो, मिलाप हुआ तत् त्वम्। असि अर्थात् 'है' इस तरह राम का अर्थ हुआ तत्त्वमसि, अर्थात् 'वह तू है।' तुम स्वयं राम हो। राम से भिन्न एक कण भी नहीं। रामोपनिषत् में है - "सत्वाच्यस्तू राकारास्यात्।"
राम कथा का स्वरूप क्या है?
जेहि महँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ।।
जिसके आदि में, मध्य में और अन्त में, भगवान राम 'मैं' आत्मा का ही दिग्दर्शन हो, अनुभूति हो यही राम कथा का स्वरूप है।
एक ही चौपाई में सातों काण्ड रामायण इस तरह है।
गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू ।।
1. गई बहोरि - बालकाण्ड है।
आशा जो चली गयी थी, वह वापस आ गयी। दशरथ की पुत्र की आशा चली गयी थी। परन्तु, पुत्र हुए और आशा लौट आयी। जनक की आशा चली गयी थी कि धनुष को अब कोई नहीं तोड सकता।
तजहु आस निज-निज गृह जाहू। लिखा न बिधि बैदेहि बिबाहू ।।
यह गयी हुई आशा वापस आ गयी।
2. गरीब निवाजू (अयोध्याकाण्ड) कहाँ केवटऔर कहाँ राम।
केवट कहता है कि -
"मोहि राम राउरि आन, दसरथ सपथ सब साची कहौं।।"
"तुम्हारे बाप की कसम खाकर कहता हूँ"
उसका ऐसा कहना भगवान राम अथवा राजा राम दोनों के पोजीशन के खिलाफ था और केवट के अधिकार के बाहर था, परन्तु राम की -
दोहा-
सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे ।
बिहसे करुना ऐन, चितइ जानकी लखन तन ।।100।।
ऐसी दृष्टि थी।
3. सरल (अरण्यकाण्ड) -
शबरी के आश्रम में भगवान राम ने जो सरलता दिखाई, वैसी सरलता सिवा भगवान राम के और कौन दिखा सकता है। शबरी में भेद का अभाव था और श्रीराम में व्यक्तित्व का अभाव था। यदि, शबरी अपने में और भगवान राम में भेद मानती कि मैं एक नीच जाति की भीलनी हूँ और ये भगवान हैं, राजा राम हैं। तो, क्या वह अपना जूठा बेर उन्हें खिला सकती थी? नहीं और राम इसी तरह अपना व्यक्तित्व रखते तो वे जूठे बेर खा सकते थे? तब दोनों में कौन-सा भाव था?
उत्तर है- "सहज सनेह" इसमें विधि-निषेध नहीं होता।
4. सबल (किष्किन्धाकाण्ड) -
दोहा-
सुनु सुग्रीव मारिहउँ, बालिहि एकहि बान ।
ब्रह्म रुद्र सरनागत, गएँ न उबरिहिं प्रान ।।6।।
विश्व विजयी बाली को, जिससे युद्ध करने जो कोई भी सामने आता था तो उसका आधा बल वह खींच लेता था, ऐसे बाली को एक ही बाण में मारूँगा, दो बाण से नहीं, ऐसा कहना यह सबलता है।
5. साहिब (सुन्दरकाण्ड) -
अगर, कोई सरकार है तो राम ही है, बाकी सब बेकार है। साहिबी यदि दिखाई है तो राम ने। समुद्र में अभी पुल बँधा नहीं, युद्ध हुआ नहीं, जय-पराजय का कुछ पता नहीं। समुद्र का जल मंगवाया और विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। तिलक सार दिया।
6. रघु (लंकाकाण्ड) -
रघु-जीव "रमुक क्रीडायां' धातु। विषयों में जो रमे, उसे रघु कहते हैं। तो, यहाँ लंका काण्ड में जो-जो मरते गये, सब रामाकार होते गये।
7. राजू (उत्तरकाण्ड) -
राजा राम की महिमा क्या थी और राम राज्य की कैसी महिमा थी, यह काण्ड इससे भरा पड़ा है।
इस रामचरित मानस में, विविध प्रकार के जो छन्द हैं, वे भाँति-भाँति की मछलियाँ हैं।
धुनि, अवरेब, कबित गुन जाती, मीन मनोहर ते बहुभाँती ।
धुनि, जो छन्द है वह रोहू मछली है। रोहू मछली खूब गहरे जल में रहती है, ये बहुत थोड़ी होती है। मानसरोवर के अन्दर रोहू क्या है? दो-दो, तीन-तीन अक्षर के छन्द जिनके शब्द थोड़े हैं। परन्तु भाव, बड़े गंभीर हैं, विस्तृत हैं। जैसे -
दोहा-
गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न ।
बंदउँ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥8।।
ये धुनि छन्द है, जो रोहू मछली के समान है। रामचरित मानस में ऐसे छन्द बहुत थोड़े हैं। अवरेव, जो छन्द हैं, वह चढ़वा मछली है, आगे का भाव पीछे को प्रकाशित करता है, जैसे- राम कथा कलि बिटप कुठारी, आदि। गुण, जो छन्द है, वह शहरी मछली है।
जैसे- "भव-भव विभव पराभव कारिनि" आदि।
जाति, जो छन्द है, वह शबरी मछली है।
जैसे-
मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुन्दर साँवरो।
अच्छा तो भैय्या! आओ, पहले राजघाट में ही स्नान करें। यह ज्ञान घाट है, जहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर स्नान करते हैं। इसको माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद कहते हैं। सन्त समाज में इस प्रसंग को "शंकर गीता" कहते हैं। लोकोक्ति है कि- बाल का आदि, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अन्त, समझै सोई सन्त। यह प्रसंग बाल का आदि ही है -
माता जी भगवान शंकर से पूछती हैं कि हे भगवन्!
प्रभु समरथ सर्वग्य सिव । सकल कला गुन धाम ।।
जोग ग्यान बैराग्य निधि । प्रनत कलपतरु नाम ।।
जौं मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिअ सत्य मोहि निज दासी ।।
तौं प्रभु हरहु मोर अग्याना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ।।
जासु भवनु सुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥
ससिभूषन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ।।
प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ।।
सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहिं रघुपति गुनगाना ।।
तुम्ह पुनि राम-राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ।
रामु सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई ।।
आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याणस्वरूप हैं। योग, ज्ञान और वैराग्य के भण्डार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है।
हे सुख स्वरूप! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने चरण की सच्ची दासी समझते हैं, तो हे नाथ! भगवान राम के प्रति मेरा जो अज्ञान है, उसे दूर कीजिये।
जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह दरिद्रता का दुःख भोगता है, यह भला कैसे संभव है? इसी प्रकार आपके चरणों के सान्निध्य में रहकर अज्ञान जनित दुःख मुझमें रहे यह कैसे सहन हो सकता है? परमारथवादी ऋषि-मुनि राम को अनादि, अजन्मा, ब्रह्म बताते हैं। शेष शारदा, वेद और पुराण जिनकी महिमा गाते हैं और फिर आप भी तो दिन-रात प्रेमपूर्वक राम-राम जपा करते हैं। तो प्रभो! क्या वे राम यही हैं, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं अथवा अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है?
दोहा-
जौं नृपतनय त ब्रह्म किमि नारि विरहँ मति भोरि ।
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ।। 108।।
चरित्र तो देखती हूँ कि "नारि विरहँ मति भोरि" स्त्री के वियोग में पागल बने पेड़-पौधे, पशु-पक्षी से पता पूछते जंगलों में भटक रहे हैं।
हे खग मृग, हे मधुकर श्रेनी, तुम्ह देखी सीता मृगनैनी ।
और महिमा सुनती हूँ कि
यद्भयाद्वाति वातोऽयं, सूर्यस्तपति यद्भयात् ।
वर्षतीन्द्रोदहत्यग्रिः मृत्युश्चरति यद्भयात् ।।
जिसके भय से वायु बहती है, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से इन्द्र वर्षा करता है और जिसके भय से काल सारे चराचर को ग्रसता है।
विधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ।।
अहिप महिप जहँ लगि प्रभु ताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥
करि विचार जिर्यं देखहु नीके । राम रजाइ सीस सब ही के ।।
तो कौन राम है? भगवन्! मेरी बुद्धि भ्रमित हो गयी है।
जौं अनीह ब्यापक बिभु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥
अग्य जानि रिस उर जनि घरहू। जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू ।।
यदि, इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ! मुझे उसे समझाकर कहिये। मुझे अज्ञ जानकर मन में क्रोध न लाइये, जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वही कीजिये।
दोहा-
बन्दउँ पद घरि घरनि सिर, विनय करउँ कर जोरि ।
बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धान्त निचोरि 109।।
हे प्रभो! मैं पृथ्वी पर सिर टेककर श्री चरणों की वन्दना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिये।
जदपि जोषिता नहिं अधिकारी। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ।।
गूढ़उ तत्त्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जहँ पावहिं ।।
यद्यपि, स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। सन्त लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ से गूढ़ तत्त्व भी उनसे नहीं छिपाते। माताजी का यह मौलिक प्रश्न है। इसी प्रश्न का उत्तर सारी रामायण है।
माताजी का कहना है कि यदि राम ब्रह्म है तो यह मनुष्यों का सा चरित्र कैसा? जिसमें योगी रमते हैं, जो व्यापक हैं, अखण्ड हैं, वे कौन राम हैं और यै कौन हैं जो "नारि विरहँ मति भोरि" आप इस तरह समझाइए कि जो वेदों का सार हो और श्रुतियों का निचोड़ हो। माता जी का प्रश्न कितनी गहराई का है। तो भैय्या! इस प्रश्न का उत्तर भी तो अत्यन्त गहराई में मिलेगा। इसीलिए, भगवान शंकर दो घड़ी ब्रह्मानन्द में डूब गये। समुद्र की तह में डूबने से ही मोती आदि बहुमूल्य रत्न मिलते हैं।
देखो भावना चार हैं-
1. असत् भावना - ईश्वर नहीं है।
2. विपरीत भावना - जीव-जीव है, ईश्वर-ईश्वर है। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है।
3. सम्भावना - शायद ईश्वर है। सम्भव तो है, पर निश्चय नहीं है।
4. असम्भावना - जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता।
भगवान आत्मा को ये भाव ढाँकने की कोशिश करते हैं। अरे! ये तो इन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकते, ढाँकना तो दूर रहा।
असत भावना वाले से यह प्रश्न है कि -
"ईश्वर नहीं है" ऐसा जो तुम कह रहे हो, तो ईश्वर के नहीं होने का अनुभव किसने किया?
उसका उत्तर है, 'मैं' ने किया।
अब विपरीत भावना वाले से प्रश्न है कि तुम जो कहते हो कि जीव-जीव है, और ईश्वर-ईश्वर है। जीव अनेक हैं और ईश्वर एक है। इस तरह जीव और ईश्वर का इस रूप में अनुभव किसने किया?
वह उत्तर देता है कि 'मैं' ने किया।
अब सम्भावना वाले से ही यही प्रश्न है, तब वह भी यही उत्तर देगा कि 'मैं' ने ही अनुभव किया है, तभी अपना अनुभव सामने रखा है, दूसरा कौन अनुभव करेगा।
अब चलो चौथे महाशय से पूछें- भैय्या! तुम जो कहते हो कि जीव कभी ईश्वरहो नहीं सकता। तुम्हारा यह कहना, सुनकर कहना है या अनुभव करके कहना है?
वह कहता है- अजी! यह हमारा अनुभव है। सुनकर क्यों कहेंगे।
तब उनसे पुनः प्रश्न है कि यह अनुभव है कि जीव कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता, किसने किया?
वह उत्तर देता है 'मैं' ने ही किया।
तब जब इन चारों भावों का अनुभव करने वाला 'मैं' आत्मा ही हुआ, इन चारों की सिद्धि 'मैं' आत्मा करके ही हुई। यदि 'मैं' न रहूँ तो अनुभव कौन करेगा? अतः, ये स्वतः सिद्ध नहीं है। अस्तित्वहीन हैं। तब, जो अस्तित्वहीन हैं, वह मुझ अस्तित्व को क्या जान सकेगा? ये 'मैं' आत्मा को किस तरह सिद्ध कर सकेंगे? जिसकी सिमि मुझ आत्मा से है, वह मुझ आत्मा को क्या ढाँकेगा? डण्डा लकड़ी को किस तरह सिद्ध कर सकेगा? क्योंकि, डण्डा है ही नहीं। वह अस्तित्वहीन है। बिना लकड़ी के उसकी सिद्ध नहीं।
1. असत् भावना का मूलोच्छेद करने वाला यजुर्वेद का महावाक्य है- 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ)।
2. विपरीत भावना का मूलोच्छेद करने वाला सामवेद का महावाक्य है- 'तत्त्वमसि' (वह तू है)।
3. सम्भावना का मूलोच्छेद करने वाला अथर्ववेद का महावाक्य है- 'अयमात्मा।' (आत्मा ही ब्रह्म है)
4. असम्भावना का मूलोच्छेद करने वाला ऋग्वेद का महावाक्य है - 'प्रज्ञानं ब्रह्मा' (तत्काल जो जानता है,
ज्ञान ही जिसका स्वरूप है)
जिस समय सीता हरण हो चुका था और उनके वियोग में भगवान राम, लक्ष्मण सहित उनकी खोज में नर-लीला कर रहे थे, उसी समय भगवान शंकर के साथ माता पार्वती ने वन में उनके इस चरित्र को देखा। उस समय राम की दशा थी -
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी । तुम्ह देखी सीता मृगनैनी ।।
खंजन सुक कपोत मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥
कुन्द कली दाड़िम दामिनी । कमल सरद ससि अहि भामिनी ।।
बरुन पास मनोज धनु हंसा । गज के हरि निज सुनत प्रसंसा ।।
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ।।
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू । हरषे सकल पाइ जनु राजू ।।
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं। प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ।।
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहुँ महा बिरही अति कामी ।।
भगवान शंकर ने जब उन्हें इस दशा में देखा तो उनने उसका अर्थ नहीं लगाया। वे जानते थे कि यह सब चरित्र असत्य और लीला मिथ्या है। अतः, मैं यदि इसका अर्थ लगाऊँगा तो मुझ पर भी कुसमय आ जायेगा। मुझे तो यार की यारी से काम है, यार के फेलों से क्या काम? अतः वे -
भरि लोचन छबि सिंधु निहारी ।
कुसमय जान न कीन्हि चिन्हारी ।।
उन्होंने कुछ हाल-चाल नहीं पूछा कि - "भगवान यह क्या बात है, आपकी यह कैसी दशा है, माता सीता कहाँ हैं? आदि।" वे जानते थे कि यदि मैंने चिन्हारी की अर्थ लगाया कि मुझ पर भी कुसमयआ जायेगा। अतः, वे इस चक्कर में नहीं पड़े और-
जय सच्चिदानंद जग पावन ।
अस कहि चलेउ मनोज नसावन ।।
वे आगे बढ़ गये। माता सती को चरित्र और लीला देख कर ही भ्रम हुआ। उसने अर्थ लगाया उसे सत्य माना, जिससे वे चक्कर में पड़ गयी।
जो तीनों काल में न हो वह असत्य है और जो न होते हुए उत्पन्न होकर नाश हो जाये वह है मिथ्या। अंधकार में रस्सी सर्प के समान दिखी रस्सी में सर्प असत्य और मिथ्या दोनों है। असत्य, इसलिए है कि सर्प तीनों काल में नहीं है। वह तो अंधकार के कारण सर्प दिख रहा है। ज्यों ही प्रकाश में देखा कि सर्पभाव चला गया। रस्सी ही रह गयी। तब, इस रस्सी में अंधकारवश सर्प हुआ और प्रकाश के आते ही उस सर्पभाव का नाश हो गया। अतः, मिथ्या है। वह रज्जू की लीला है। जो जिसमें भासै, वही उसका चरित्र है। सर्प रज्जू में भासता है, अतः सर्प रज्जू का चरित्र है। सर्प न तो अंधकार में है और न प्रकाश में है, अतः असत्य है। इसी तरह 'मैं' आत्मा भगवान में जगत् प्रपंच का अज्ञान के अन्धकार में भासना, यह मुझ आत्मा 'मैं' का चरित्र है, जो असत्य है।
सर्प नहीं होते हुए भी सर्प भासना, जो कि भय कम्पन का कारण है, वह भासता क्यों है? अरे! यही तो रज्जू की लीला है, जो मिथ्या है। मुझ आत्मा 'मैं' में जगत् प्रपंच नहीं होते हुए भी, जो सारे द्वंद्वों का कारण होता है, क्यों भासता है? अरे, यही तो मुझ आत्मा 'मैं' की लीला है। जो नहीं है वह सर्प है, जगत् प्रपंच है, यह असत्य है, यही चरित्र है और नहीं होते हुए भी जो भासता है, सर्प, प्रपंच, यह मिथ्या है, यही तो मुझ आत्मा 'मैं' की लीला है। अभाव को देखकर, सुनकर भ्रम होता है, भाव को नहीं। सर्प अभाव रूप है और रज्जू भाव रूप है। वही देखा जाता है, जो कभी न हो, रज्जू में सर्प देखा गया जो कभी नहीं है। जो दिखता है वह विकल्प है, वही जगत् है। विकल्प कहते हैं- योग दर्शन का सूत्र है-
"शब्द ज्ञानानुपाती, वस्तु शून्यो विकल्पः ।''
अर्थात्, जिससे केवल शब्द मात्र का ही ज्ञान हो और वस्तु का अभाव हो, उसे विकल्प कहते हैं। जैसे-डण्डा शब्द सुन पड़ा, परन्तु ढूँढने चलेंगे तो हाथ में केवल लकड़ी ही लकड़ी लगेगी। डण्डा नाम की कोई चीज मिलने वाली नहीं है। डण्डा अस्तित्वहीन अभाव रूप है, जो है ही नहीं। मतलब यह कि अस्तित्वहीन पदार्थ जो किसी भी काल में न मिले उसे ही विकल्प कहते हैं। सर्प विकल्प है, वही जगत् है। अनुभव उसी का होता है, जो त्रिकालाबाध्य हो, अभाव न हो। जो भाव है, वह मैं 'है' है, आत्मा है और जो 'है' है अस्तित्व, वह राम है। जो राम है, वह त्रिकालाबाध्य है। यह ज्ञान के प्रकाश से जाना जाता है। भगवान शंकर के लिए चरित्र असत्य और लीला मिथ्या थी, यह ज्ञान के प्रकाश में देखा गया। अतः, वे भ्रम, शोक और मोह से रहित रहे। परन्तु, माता सती भ्रम में पड़ गयी, जिससे उन्हें मोह हुआ, जो दुःख का कारण हुआ। यह अज्ञान के अन्धकार में दिखा! मृगजल, दिखता दोनों को है, जिसे सूर्य की सत्ता का ज्ञान है उसे और अज्ञान है उसे भी, परन्तु अज्ञानी उसे मृग के समान सत्य जल मानता है और ज्ञानी उसे सूर्य की सत्ता जानता है, जल का अभाव जानता है। एक के लिए प्रत्यक्ष जल है और दूसरे के लिए सूर्य की सत्ता है। जिसको सत्य भासता है, उसके लिए दुःख रूप है और जिसको सत्ता भासता है, उसके लिए वह सुख रूप है।
'मैं' आत्मा की सत्ता करके, यह जगत् प्रपंच भासता है। मृग, जल मानकर दौड़ता है, जानकर नहीं। इसी प्रकार यह जगत् प्रपंच, 'मैं' आत्मा भगवान राम की सत्ता है इसे मानकर नहीं, जानकर चलो।
भैय्या! चरित्र असत्य और लीला मिथ्या है। एक बार राम दरबार लगा हुआ था। भगवान राम और माता सीता सिंहासन पर बैठे हुए थे कि भक्त शिरोमणि हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हुए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े हुए देख, भगवान राम ने माता सीत से कहा- सीते, देखो सामने हाथ जोड़े हुए हनुमान जी खड़े हुए हैं। वे आत्म तत्त्व की जिज्ञासा से खड़े हैं। वे इस तत्त्व के जानने के पूर्ण अधिकारी हैं। अतः, तुम मेरे स्वरूप परम तत्त्व का उनके समक्ष विवेचन करो। रामाज्ञा को स्वीकार कर जगत जननी सीता देवी श्री हनुमान जी से कहने लगीं- हे हनुमान जी!
रामं विद्धि परब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् ।
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम् ।।
आनन्दं निर्मलं शातं निर्विकारं निरंजनम् ।
सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम् ।।
श्रीराम को सच्चिदानंद विग्रह, सारी उपाधियों से रहित, सत्तामात्र, इन्द्रियातीत, आनन्दमूर्ति, शुद्ध, शान्त, विकार शून्य, निरंजन अर्थात् निर्लेप, सर्वव्यापी, स्वयंप्रकाश, कल्मषहीन अर्थात् दुःखों से रहित, आत्म स्वरूप, अद्वितीय परब्रह ही समझो।
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच -
त्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किञ्चित् ।
आनन्दमूर्ति रचलः परिणामहीनो,
मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति ।।
रामः परमात्मा पुरुषः पुराणो,
नित्योदितो नित्यसुखो निरीहः !
तथापि माया गुणसं गतो सौ
सुखीव दुःखीव विभाव्यते बुधैः ।।
श्रीराम न तो कहीं जाते हैं, न कहीं ठहरते हैं, न किसी के लिए शोक करते हैं, न किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, न किसी का परित्याग करते हैं, न कोई कर्म करते हैं, वे तो अचल, आनन्दमूर्ति एवं परिणामहीन हैं, अर्थात् उनमें परिवर्तन नहीं होता, केवल माया के गुणों के संबंध से, उनके अन्दर ये बातें होती हुई सी प्रतीत होती हैं। श्रीराम परमात्मा, पुराण पुरुषोत्तम, नित्य प्रकाशित, नित्य सुख से सम्पन्न एवं निरीह अर्थात् चेष्टा से रहित हैं, किन्तु फिर भी माया के गुणों से सम्बद्ध होने के कारण, उन्हें बुद्धिमान लोग सुखी अथवा दुःखी समझ लेते हैं।
तीनों गुणों (सत्, रज, तम) से युक्त मैं मूल प्रकृति हूँ। मुझ माया में ऐसी कुछ शक्ति नहीं है कि मैं स्वयं कुछ कर सकूँ। भगवान राम के सन्निकट रहकर ही मैं सब कुछ करती हूँ। राम अकर्त्ता हैं, अभोक्ता हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं। मैं प्रकृति माया हूँ। जिस तरह चुम्बक के कारण लोहा भी कर्त्तापन को प्राप्त होता है, इसी प्रकार में भगवान राम के आश्रय से कुछ कर सकने में समर्थ हूँ।
मुझ माया का रामावतार हुआ है। सारा चरित्र मैंने ही किया, राम ने नहीं। विश्वामित्र के मख की रक्षा मैंने की। जनकपुर से धनुष मैंने तोड़ा। सीता का विवाह मुझसे हुआ। चौदह वर्ष के लिए बनवास मुझे हुआ। वन में गयी। सुग्रीव से मित्रता मैंने की। शबरी के बेर मैंने खाये, रावण से युद्ध मैंने किया। राम राज्याभिषेक मेरा हुआ, राम का नहीं। इस प्रकार राम जन्म से लेकर अन्त तक, सारा चरित्र मेरा ही है। सारा चरित्र माया किया राम ने नहीं। राम तो सर्वव्यापक है, आनंद ही इनका स्वरूप है। आनंदमूर्ति राम मुझ माया में व्यापक हैं। अतः, वे मुझ माया में भासते हैं। यह सब मैंने ही किया राम ने नहीं। देहाभिमानी को ही यह सब चरित्र सत्य दिखता है, तत्त्ववित् आत्मनैष्ठिको को नहीं। राम अक्रिय हैं, वे जरा भी कुछ नहीं करते। वे अचल हैं, एक रस हैं। जितर सब चरित्र जन्म से लेकर अंत तक सम्पूर्ण हुआ, कुछ नहीं।
दोहा-
मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह ।
रघुपति चरित महेस तब, हरषित बरनै लीन्ह ||111||
भगवान शंकर ने दो घड़ी आनन्द सागर में डूबकी लगाई, तब क्या रत्न मिला वो बाहर आकर कहते हैं कि हे पार्वती! तुमने जो चरित्र देखा, वह क्या देखा? किसमे देखा? किसको देखा? किसने देखा?
जिसको बिना जाने, झूठ भी, अभाव रूप भी जो है ही नहीं, वह सत्य सा भासता है। बिना रस्सी के जाने, सर्प जो अभाव रूप है, है ही नहीं। वह सत्य सा भासता है, प्रतीत होता है। रस्सी को जान लो, जो कि सर्प का आधार है। (क्योंकि यदि रस्सी न होगी, तो सर्प दिखेगा किसमें?) तो सर्प का अभाव हो गया। जिसमे दिखता है, उसके आधार को जान लो, फिर देखने का अभाव हो गया। डण्डा दिख रहा है, इसका आधार लकडी को जान लो, फिर डण्डे का अभाव हो गया। लकड़ी ही दिख रही है। डण्डा तो विकल्प था, अस्तित्वहीन जो है ही नहीं।
जो दिखता है, वह दिखता है, मैं दिखता हूँ तब दिखता है।
इस रहस्य को जान लिया, फिर दिखना कहाँ, जो दिखता है।।
लकड़ी यदि न दिखे, तो डण्डा कैसे दिखे। भाई देखने वाला ही दिखता है, दूसरा नहीं। द्रष्टा ही दृश्य है। नहीं होते हुए जो भासता है, वह भगवान का चरित्र है, जो विशद और विमल है। मुझ आत्मा 'मैं' में यह प्रपंच (राम चरित्र) नहीं होते हुए भी दिखा, क्यों? अरे, यही तो उसकी लीला है, यह सब अज्ञान के अन्धकार में अज्ञानी जनों को दिखता है। तत्त्ववित् को नहीं।
झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ।।
जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन भ्रम जाई ।।
हे पार्वती! तुमने झूठे को देखा, अभाव को देखा और उसके आधार के अज्ञान में जो दिखा उसे सत्य मान लिया, जिसके जान लेने पर संसार प्रपंच का अभाव हो जाता है, वह आधार भगवान आत्मा 'मैं' है। चराचर का अस्तित्व अपना आप, जो हर एक के भीतर 'मैं' हूँ, 'मैं' हूँ ऐसा रात-दिन बोल रहा है, उसके बिना जाने यह संसार प्रपंच मन, बुद्धि, शरीर आदि जो तीन काल में है ही नहीं, सत्य-सा जान पड़ता है।
भाई, यही श्रुतियों, स्मृतियों के सिद्धांत का निचोड़ है, जिसे भगवान शंकर ने ब्रह्मानंद, आत्मानंद, निजानंद, नित्यानंद, सागर में दो घड़ी डूबकर, गोता लगाकर, बाहर निकाला। कौड़ी, घोंघी, सीप और शंखियाँ आदि तो समुद्र के बाहर किनारे में भी मिल जाती हैं, परन्तु यदि अमूल्यरत्न निकालना है, तो भैया! इसके लिए तो समुद्र की तह में, गहरे जल में मीलों जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मिलेगा। इसी तरह माताजी का प्रश्न कोई किस्सा-कहानी, राजा-रानी के चरित्र, इतिहास आदि जानने को होता तो, भोले बाबा को दो घड़ी समाधिस्थ होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर, यहाँ तो माता जी ने कहा था कि भगवन्! आप वेदों, शास्त्रों का सार तथा श्रुतियों स्मृतियों के सिद्धान्त का निचोड़ कहिए। भगवान शंकर कहते हैं- जैसे- जागने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है, उसी प्रकार स्व स्वरूप भगवान आत्मा 'मैं' के जान लेने पर संसार प्रपंच का अभाव हो जाता है।
जिस समय मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब वह यह नहीं जानता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, यह असत्य है, जागने पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, उससे यदि जाग्रत अवस्था का मनुष्य कहे कि भाई! यह तू जो देख रहा है, वह असत्य है, स्वप्न है, तो वह उस समय कदापि नहीं मानेगा, क्योंकि वह उस अवस्था में, जाग्रत की नाई सब प्रत्यक्ष ही सत्य देख रहा है, परन्तु वही मनुष्य जब जाग जाता है, तब अपने आप ही कहता है कि आज मैंने ऐसा देखा वह स्वप्न था, आदि। उसे यह समझाना या बताना नहीं पड़ता कि यह असत्य है। झूठ को तुमने देखा था और सत्य माना था। स्वप्नकाल में वह उसके लिए सत्य ही था, वह तो जागने पर असत्य हुआ, इसी तरह स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जाग जाओ, तो इस जगत् प्रपंच का अपने आप अभाव हो जायगा।
जो सपने सिर काटै कोई। बिनु जागे न दूरि दुख होई ।।
तुलसीदास जी ने विनय में कहा है -
मैं हरि, साधन करइ न जानी।
जस आमय भेषज न कीन्ह तस, दोष कहा दिरमानी ।।
सपने नृप कहँ घटै बिप्र-बघ, बिकल फिरै अघ लागे ।
बाजिमेध सत कोटि करै, नहिं सुद्ध होइ बिनु जागे ।।
हे प्रभो ! मैंने साधन करना नहीं जाना, जैसा रोग था वैसी दवा नहीं की। इसमें इलाज का क्या दोष? जैसे सपने में किसी राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाय और वह उस महापाप के कारण व्याकुल, जहाँ-तहाँ भटकता फिरे, परन्तु जब तक वह जागेगा नहीं, तब तक सौ करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने पर भी वह शुद्ध नहीं होगा, इसी प्रकार भगवान 'आत्मा' स्वस्वरूप 'मैं' में बिना जागे अज्ञान जनित संसार प्रपंच से छुटकारा नहीं मिल सकता।
स्रग-महँ सर्प बिपुल भय दायक, प्रगट होइ अबिचारे ।
बहु आयुध घरि, बल अनेक करि, हारहिं मरइ न मारे ।।
जैसे अंधकार में रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है और वह (मिथ्या सर्प का भ्रम न मिटने तक) अनेक हथियारों के द्वारा बलपूर्वक मारते-मारते थक जाने पर भी नहीं मरता। अरे यार! साँप होता तब तो मरता, जब है ही नहीं तब मरेगा क्या? इसी प्रकार-अज्ञान से भासने वाला यह संसार, बिना इसके असली स्वरूप के जाने नष्ट कैसे होगा ?
निज भ्रम ते रबिकर-सम्भव, सागर अति भय उपजावै ।
अवगाहत बोहित नौका चढ़ि, कबहूँ पार न पावै ।।
अपने ही भ्रम से सूर्य किरणों से उत्पन्न हुआ मृगतृष्णा का समुद्र बड़ा ही भयावना लग रहा है और उस मिथ्या सागर में डूबा हुआ मनुष्य क्या जहाज या नाव पर चढकर पार पा सकता है? नहीं, यही हाल इस अज्ञान से उत्पन्न संसार सागर का है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक 'मैं' पर जितनी मान्यताएँ हैं, विकल्प हैं, अमुक भाव हैं, इनका अत्यन्ताभाव न हो जाये, तब तक करोड़ों यत्न करके भले मर जाओ, परन्तु इस संसार सागर से पार नहीं पा सकते। अमुक भाव, विकल्प भाव ही तो संसार है। अमुक भाव गया कि संसार न रहा। जब संसार का, अर्थात् विकल्प का अभाव हो गया तब विकल्प ही कहाँ रहा? विकल्प के अभाव में विकल्पक का भी अभाव हो गया। विकल्पक संज्ञा न रहा, पर जिस पर ये दोनों कल्पित थे वह रहा, जिसमें दोनों आधारित थे।
किसी व्यक्ति की शादी हुई, गृहणी आयी, अभी वह व्यक्ति ही है, परन्तु जिस क्षण पुत्र हुआ उस व्यक्ति का नाम पिता हो गया। पुत्र के होते ही पिता नाम पड़ गया, अब जिस दिन पुत्र मर गया, पुत्र न रहा उसी क्षण, उसी दिन से पिता भी न रहा। पुत्र के अभाव में पिता कहेगा कौन? अतः, पिता भी जाता रहा, परन्तु वह व्यक्ति तो रहा, उसका अभाव नहीं हुआ। उसी पर पिता-पुत्र दोनों कल्पित थे। केवल पिता संज्ञा न रहा।
इसी तरह विकल्पक 'मैं' और विकल्प हुआ संसार। विकल्प का ज्योंहि अभाव हुआ कि विकल्पक का भी अभाव हो गया, परन्तु 'मैं' रहा, जिस पर दोनों आधारित थे।
यही - तुलसीदास जग आपु सहित जब लगि निरमूल न जाई का भाव है। कर्म देश में जगत्, उपासना देश में चरित्र, ज्ञानदेश में ब्रह्म और तत्त्व देश में 'मैं', कर्म में जो अकर्म और अकर्म में जो कर्म देखता है, वही ज्ञानवान है। कर्म हुआ जगत्, अकर्म हुआ 'मैं' आत्मा। कर्म देश में जगत् दिखता है और 'मैं' आत्मा आत्मदेश में जगत् का अत्यन्ताभाव है।
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई ।।
अपने आत्म स्वरूप 'मैं' आत्मा के बोध हो जाने पर, फिर संसार प्रपंच का अत्यन्ताभाव हो जाता है। विकल्प, मान्यता, अमुक भाव, माया, मन, संसार सबका एक ही भाव है। ये एक ही के पर्यायवाची शब्द हैं।
जो माना जाय, वह है-माया। जिसको माना जाय, वह है उसका आधार, स्वामी, पति, रक्षक अर्थात् माया-पति।
डण्डा, यह माना गया है। यह है माया। डण्डा किसको माना गया? लकड़ी को। तब लकड़ी है डण्डे का आधार, डण्डे का पति, रक्षक, स्वामी। पति का अर्थ होता है रक्षक। यदि डण्डा से लकड़ी निकाल लोगे तो डण्डा का अस्तित्व ही खतम हो जायगा। वह रहेगा किसमें? डण्डा कहा किसको जायगा? अतः लकड़ी डण्डे का आधार हुई, पति हुई, स्वामी और रक्षक हुई। बिना लकड़ी के डण्डा एक क्षण भी जिन्दा नहीं रह सकता। लकड़ी मायापति हुई। अब डण्डे की मान्यता से लकड़ी ढँक गयी, डण्डे ने लकड़ी को छिपा लिया, माया से मायापति ढँक गया। इस प्रकार 'मैं' आत्मा पर जितनी मान्यताएँ हैं, उन मान्यताओं से, माया से 'मैं' आत्मा ढँक गया। माया अपने आधार को अधिष्ठान को, ढाँक कर छिपा लेती है।
माया से मायापति 'मैं' आत्मा भगवान छिप गया।
'मैं' हूँ, अब इस 'मैं' आत्मा पर जितनी मान्यताएँ हुई, जितने विकल्प हुए, जो-जो अमुक भाव आया, 'मैं' को जो-जो माना गया, उन-उनसे 'मैं' आत्मा ढँक गया। क्या-क्या मान्यताएँ हुई?
'मैं' देह हूँ। 'मैं' पर देह की मान्यता हुई। 'मैं' को देह माना। देह मानने के बाद फिर माना कि 'मैं' स्त्री हूँ, 'मैं' पुरुष हूँ। 'मैं' बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ। आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जन्मता हूँ, मरता हूँ। ब्राह्मण हूँ, क्षत्री हूँ, वैश्य हूँ, शुद्र हूँ, माता, पिता, भाई, बहन, मामा, चाचा, पुत्र हूँ। गृहस्थी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, वानप्रस्थी हूँ, संन्यासी हूँ आदि अनेक मान्यताएँ 'मैं' पर होती गयी। इन मान्यताओं से 'मैं' आत्मा ढँक गया। ढक्कन ही माया है और जो ढँका है, वह मायापति भगवान है।
'मैं' जीव हूँ। 'मैं' को जीव मान लिया। इस जीव मान्यता के बाद 'मैं' सुखी हूँ, दुखी हूँ। पुण्यी हूँ, पापी हूँ, स्वर्गी हूँ, नर्की हूँ आदि अनेक अमुक भाव 'मैं' पर लद गये जिससे 'मैं' आत्मा छिप गया। 'मैं' पर माया का ढक्कन पड़ गया।
मैं 'ब्रह्म' हूँ। 'मैं' को ब्रह्म मान लिया गया। इस ब्रह्म की मान्यता के बाद 'मैं' द्रष्टा हूँ, 'मैं' साक्षी हूँ, 'मैं' नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन, निराकार, निर्लेप, निरीह हूँ, निर्मल हूँ, निर्विकार हूँ, अनन्त हूँ, अपार हूँ, पूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ आदि अनेक मान्यताएँ आ गयी। इन मान्यताओं से 'मैं' आत्मा ढँक गया। 'मैं' पर पर्दा पड गया। 'मैं' छिप गया।
'मैं' आत्मा कहा जाता है: प्रश्न है 'मैं' को आत्मा क्यों माना? अरे भाई! 'मैं' और आत्मा, भिन्न-भिन्न नहीं हैं। आत्मा का नाम अस्तित्व है। 'है' है, यह सामान्य चेतन सारे चराचर में व्यापक है। यह भगवान का अव्यक्त रूप है और 'मैं' यह विशेष चेतन है, व्यक्त रूप है। जो अव्यक्त रूप 'है' है, उसका ही व्यक्त रूप 'मैं' है। 'है' ही है, जो अपने को 'मैं' नाम से व्यक्त कर रहा है। इस तरह दोनों एक ही हैं, अलग- अलग नहीं।
आत्मा के लिए 'मैं' कहना ही पर्याप्त है, परन्तु अनादि काल से 'मैं' को देह माने बैठे हैं, देह से अलग होना ही नहीं चाहते। अतः 'मैं' के साथ आत्मा लगाकर कहना पड़ता है। जितनी मान्यताएँ हैं, यही माया देश है, अमुक देश है, परदेश है, जीव जगत् है, प्रपंच देश है, विकल्प देश है, यही अज्ञान जगत् है। इन सब मान्यताओं को हटा दो। बस, अब जो शेष रह गया 'मैं' आत्मा, यही आत्मा देश है, स्वदेश है, भगवान देश है, ज्ञान जगत् है।
यदि लकड़ी न होगी, तो डण्डा मानोगे किसको ? रस्सी न होगी तो अंधेरे में सर्प किसको कहोगे? तब लकड़ी को ही डण्डा माना गया, रस्सी को ही सर्प माना गया। इसी तरह 'मैं' आत्मा को ही, माया माना गया। यदि 'मैं' आत्मा न होऊँ, तो माया का आधार कौन होगा? किसको माना जायेगा? देह हूँ, जीव हूँ, ब्रह्म हूँ आदि मान्यताएँ, किस पर की जाएंगी?
जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प का भ्रम दूर हो जाता है। अरे, यह तो रस्सी ही है, जिसको मैंने सर्प मान लिया था। इस भ्रम का कारण था अंधकार। अन्धकार दूर होते ही, रस्सी प्रत्यक्ष दिखने लगी, इसलिए सबसे पहिले अन्धकार को ही दूर करना पड़ेगा। इधर अंधेरे का नाश हुआ कि उधर रस्सी का ज्ञान हो गया। दोनों साथ ही साथ हुआ। इसी प्रकार सर्प रूप इस संसार प्रपंच का कारण अज्ञान, अंधकार है, ज्यों ही ज्ञान का प्रकाश हुआ कि अज्ञान का नाश हो गया अर्थात् 'मैं' आत्मा का बोध हो गया। स्वरूप आत्मा के बोध में जगत् प्रपंच नहीं है।
झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें ॥
यही रघुनाथ जी का विमल यश है कि तीन काल में कुछ हुआ ही नहीं। नाम रूप संसार है, नाम सुना जाता है और रूप देखा जाता है। बस, यही संसार है। हृदय में संसार का प्रवेश दो इन्द्रियों के द्वारा होता है, देखकर और सुनकर -
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ।।
बुध, अर्थात् विवेकी, ज्ञानी जन, सुखी होते हैं, क्योंकि चरित्र को देखकर और सुनकर भी वे जानते हैं कि न कुछ हुआ है, न हो रहा है और न कुछ होने वाला है, जैसे कि शिवजी को हुआ। चरित्र को देखकर और सुनकर भी वे -
जय सच्चिदानन्द जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ।।
कहकर आगे बढ़ गये, उन्हें न तो हर्ष हुआ, न विषाद और न विस्मय तथा मोह ही। रस्सी में सर्प असत्य है, क्योंकि यदि सत्य होता तो प्रकाश में भी दिखता, परन्तु प्रकाश में सर्प नहीं दिखता। अतः, सर्प सत्य नहीं है, तब क्या असत्य है? अरे, असत्य होता तो देखने से भय, कम्पन नहीं होता। अतः, असत्य भी नहीं है। चरित्र को सत्य कहो तो बनता नहीं, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता, वह तीनों काल और तीनों अवस्था में नित्य एक रस रहता है तभी तो सत्य है, परन्तु चरित्र तो नित्य नहीं है उसका अभाव हो जाता है, अतः सत्य नहीं है। जब चरित्र सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, सत्यासत्य नहीं है, क्योंकि साधक-बाधक पदार्थ एक साथ नहीं रह सकते, तब क्या है? इस पर भगवान शंकर कहते हैं कि यह तर्क का विषय नहीं है।
सगुन राम के चरित भवानी, तरकि न सकहिं बुद्धि मन बानी ।।
भगवान के चरित्र में तर्क की गुंजाइश नहीं है। तर्क में गुण-दोष आता है और भगवान गुण-दोष से परे हैं। इस तरह चरित्र क्या है? कुछ कहते नहीं बनता।
भाई! जब जिसका चरित्र है, वही मन वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है, तब उसका चरित्र ही कैसे वचनीय होगा, वह भी अनिर्वचनीय है!
जिस आधार पर माना जाय वह आधार 'मैं' आत्मा है, जो माना जाय, वह है माया। जब तक मान्यता है, रजोगुण युक्त सृष्टि का पालन है। जब मान्यता समाप्त हो जाय अर्थात् मान्यता का अभाव ही रजोगुण युक्त सृष्टि का संहार है। तीनों गुणों के समुच्चय का नाम माया है, तीनों गुण अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
'मैं' भगवान आत्मदेश में 'मैं' आत्मा भगवान के जन्म, कर्म का अत्यंताभाव है, यही 'मैं' आत्मा भगवान का दिव्य जन्म कर्म है, यह हुआ बोध। इस बोध के बोध को, जो बोध से जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बोध को ही प्राप्त होता है।
राम सरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर ।
अबिगत अकथ अपार, नेति, नेति नित, निगम कह ||26||
हे राम! तुम्हारा रूप, 'स्व' रूप है, यदि 'पर' रूप होता तो कहने में आता। स्व = स्वयं 'मैं'। न मैं बद्ध हूँ, न तुम मुक्त हो, न मैं ज्ञानी हूँ, न तुम अज्ञानी हो, न मैं ब्रह्म हूँ, न तुम जीव हो। न मैं सेवक हूँ, न तुम सेव्य हो, इन समस्त भावों के अभाव का जो भाव है वह राम का जानना है, यह बुद्धिगम्य, इन्द्रियगम्य, वाणीगम्य नहीं है। नहीं, नहीं को देखता है और है, है को देखता है। संशय-विपर्यय के अभाव का नाम ही अनुभव है। यह है अथवा नहीं, इसका नाम संशय (अनिश्चय का नाम)। यह, नहीं है, दूसरा है अर्थात् अन्य को अन्य समझना, इसका नाम विपर्यय है (विपरीत ज्ञान)। अनुभवगम्य के अनुभव में संशय विपर्यय का अभाव है। यही रघुनाथजी का विमल यश है और श्रुतियों, स्मृतियों के सिद्धान्त का निचोड़ है। ये चीजें तह में डूबने से मिलती हैं, जिसे भगवान शंकर ने डुबकी लगाकर निकाला।
चरित्र में जो अनिर्वचनीयता है, वह चरित्र का है या जिसका चरित्र है, उसका है। उत्तर है-जिसका चरित्र है, उसका है। अंगूठी में जो पीलापन है, वह अंगूठी का है या सोने का? उत्तर है-सोने का है। (अंगूठी, सोने का चरित्र है)
असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी ।।
दनुज कहते हैं देहाभिमानी को, जिसने देह को ही अपना स्वरूप मान लिया है और जन कहते हैं, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है।
भगवान का चरित्र स्वरूप ज्ञानियों के लिए सुखदाई है और अज्ञानियों के लिए, दुःखदाई है।
जथा अनेक बेष घरि, नृत्य करइ नट कोइ ।
सोइ सोइ भाव दिखावइ, आपुन होइ न सोइ ।।
यह संसार नाट्य शाला है, यहाँ वह खुद ही तो नाटककार है, खुद ही तो सूत्रधार है, खुद ही राजा है, खुद ही रानी है, खुद ही तो दास है, खुद ही दासी है, खुद ही चोर है, खुद ही साव है, खुद ही साधू है, खुद ही चाण्डाल है, खुद ही पापी है, खुद ही पुण्यात्मा है, खुद ही नीं है, खुद ही स्वर्गी है, नाटकशाला रूप संसार भी खुद ही है। मगर "आपुन होइ न सोइ । भैय्या! विचित्र महिमा है, कहाँ तक कहें -
कहीं होय विरंचि सृष्टि रचता अनेक भाँति,
कहीं होय मुकुन्द सृष्टि पालत अपेला है।
कहीं होय महेश भेष, सृष्टि खास नाश करै,
या प्रकार तीन रूप धरै, तीन बेला है ।
कहीं जै गोविन्द देव वृन्द होय अनन्द करै,
कहीं बन दैत्य देव झगर झमेला है ।
कहाँ लौ बखानिये, न जानिये, सो वाकी गति,
है सही अकेला, पै अनेक खेल खेला है।
स्वयं ही खिलाड़ी है, स्वयं ही खेल है और स्वयं ही दर्शक है। द्रष्टा, दृश्य, दर्शन सब स्वयं ही है।
नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवकहिं न ब्यापै माया।
सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला, जापर हो सो नट अनुकूला ।।
यहाँ पर भगवान की उपमा इन्द्रजाली से दी गयी है, इन्द्रजाली का प्रत्येक खेल विचित्र और प्रत्यक्ष होता है। इस खेल को देखकर वही विस्मय में नहीं पड़ता, जो उसका कृपा-पात्र होता है। बाकी सबको यह इन्द्रजाली अपने इन कपट भरे खेलों से विमोहित कर लेता है। उसके सभी खेल कपट पूर्ण होते हैं, अर्थात् असत्य होता है, परन्तु बिना इन्द्रजाली की कृपा के उसका भेद (रहस्य) समझ में नहीं आता और सत्य ही प्रतीत होता है।
एक बार इलाहाबाद में बैंक के पीछे पोलो ग्राउण्ड में इन्द्रजाली का खेल हुआ। इन्द्रजाली ने अपना खेल दिखाने के पूर्व, कलेक्टर से स्वीकृति ले ली थी। बाद में अपना खेल दिखाया। इस खेल के लिए टिकट की व्यवस्था थी और बड़े-बड़े लोग बहुत संख्या में इस खेल को देखने आये थे। उसका खेल इस प्रकार था -
इन्द्रजाली जोर-जोर से डमरू बजाने लगा और उसकी स्त्री ढोलक बजाने लगी। इन दोनों बाजों की आवाज से दर्शकों का मन उनकी ओर केन्द्रित हो गया। इतने में दर्शकों ने सुना कि आकाश मंडल में मारो-मारो, दौड़ो, राजा रामचन्द्र की जय, लंकापति रावण की जै आदि आवाज जोर-जोर से आने लगी। तब इन्द्रजाली ने अपनी स्त्री से कहा, सुन रही हो, क्या आवाज आ रही है? स्त्री कहने लगी-सुन तो रही हूँ। यह काहे की आवाज है? जो लगातार आ रही है और बड़ी मारकाट मची हुई है।
इन्द्रजाली कहने लगा- अरी पगली ! तू क्या जानेगी। राम-रावण का घोर युद्ध हो रहा है और मेरा भी बुलौवा आ गया है। मुझे भी वहाँ जाना जरूरी है। देखो अब मैं चला। ऐसा कहकर उसने कच्चे तागे की एक बिल्कुल पतली गड्डी अपनी झोली से निकाला और उसके एक छोर को अपने हाथ में रखकर पूरी गड्डी को आकाश मंडल की ओर फेंक दिया। गड्डी सर्र से आकाश की ओर चल दी और कच्चे धागे का लंब खड़ा हो गया। अब इस लंब रूप धागे को पकड़कर इन्द्रजाली आकाश मण्डल की ओर चढने लगा। सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो, कौतूहलपूर्ण दृष्टि से उस ओर देखते रहे। लगभग डेढ फर्लांग तक वह इन्द्रजाली धागे के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया, बाद में वह आँखों से ओझल हो गया। मारकाट की आवाज पूर्ववत् आ रही थी। इतने में दर्शकों ने देखा कि इन्द्रजाली का एक हाथ कटकर उसकी स्त्री के पास गिरा। स्त्री छाती पीटकर, ढांडे मार-मारकर, चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगी। वह रो-रोकर कहते जाती थी कि मैं लुट गयी, मेरा सहारा छिन गया, मैं बेमौत मारी गयी। अब संसार में मेरा आश्रय कौन है? इतने में उसके पति का दूसरा हाथ भी कटकर उसके समीप गिरा, स्त्री इसी तरह और जोर-जोर से रोने लगी। फिर इन्द्रजाली के दोनों पैर कटकर भूमि पर गिरे और थोड़ी देर बाद उसका सिर कटकर उसकी स्त्री की गोद में गिरा। दर्शक यह सब दृश्य देखकर करुणा और आश्चर्य में डूब गये।
अब स्त्री ने कहा कि जब संसार में मेरा पति ही नहीं रहा, तब मैं ही जीकर क्या करूँगी। भाइयों! जल्दी चिता बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करो, मुझे अपने पति की लाश को गोद में लेकर सती होना है। तुरन्त, लकड़ी की व्यवस्था कर चिता बनायी गयी और सबके देखते-देखते, वह स्त्री अपने पति के कटे हुए अंगों को गोद में लेकर चिता में बैठ गयी और जलकर राख हो गयी। कैसा हृदय विदारक कारुणिक दृश्य था। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न था। एक दस मिनट के बाद ही लोगों ने देखा कि वे दोनों स्त्री-पुरुष एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक ओर से चले आ रहे हैं और वे सब दर्शकों के बीच उपस्थित हो गये। बस, फिर क्या था, इस दृश्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हजारों रुपयों की भेंट व न्यौछावर उस खेल पर किये गये। किसी ने अपने हाथ की घड़ी निकाल कर दे दी, किसी ने सोने का अपना चेन दे दिया, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी अपने गले का हार एवं अन्य आभूषण उस इन्द्रजाली को भेंट में दे दिया। इस तरह सबों की जेब खाली हो गयी।
सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला। जापर होइ सो नट अनुकूला ।।
मान्यता इन्द्रजाल है, मान्यता का आधार 'मैं' आत्मा इन्द्रजाली है।
इन्द्रजाली रूप मुझ आत्मा में, इन्द्रजाल रूप यह प्रपंच असत्य होते हुए, सत्य भासता है।
अव्यक्त रूप से जो सर्व का 'है' है और व्यक्त रूप से जो सर्व का 'मैं' है, उस 'मैं' आत्मा की जिस पर असीम कृपा है, वह इस प्रपंच के रहस्य को जानकर, उससे प्रभावित नहीं हो सकता।
इसी तरह भगवान राम, इन्द्रजाली चरित्र हैं, इसे देखकर वही विमोहित नहीं होते, जिन पर भगवान राम इन्द्रजाली की कृपा है, यही उनका विमल यश है तथा श्रुतियों, स्मृतियों के सिद्धांत का निचोड है कि तीनों काल में कुछ हुआ ही नहीं।
झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें ।।
भगवान शंकर ने निजानन्द सागर में डुबकी लगाई, तो यही रत्न लेकर वे बाहर आये। जिसको जगत् कहते हो, यही रघुनाथजी का विमल यश है। रज्जू के अज्ञान में, जैसे सर्प भासता है, उसी प्रकार भगवान आत्मा के अज्ञान में, जगत् प्रपंच भासता है।
जिस तरह रज्जू की सत्ता से सर्प की सत्ता भिन्न नहीं है, अर्थात् रज्जू ही तो है, जो सर्प के रूप में दिख रहा है, इसी तरह जगत् प्रपंच भी मुझ आत्मा 'मैं' की सत्ता से भिन्न नहीं है। यदि 'मैं' आत्मा जगत् प्रपंच से भिन्न होता, तो मैं प्रपंच का अनुभव नहीं कर सकता और अभिन्न होता, तो भी मैं प्रपंच का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि एक में अनुभव कहाँ? अतः, विषय प्रपंच का अनुभव करने के लिए 'मैं' प्रपंच होकर ही उसका अनुभव करता हूँ।
देखो! मेला में लाखों मनुष्य उपस्थित हैं, उनमें से प्रत्येक से पूछो, भाई! तुम कहाँ आये हो? तो प्रत्येक यही जवाब देगा "मेला देखने। अब विचार करो कि ये जितने भी मनुष्य मेला में हैं, वे सब तो मेला देखने वाले हुए, अब मेला कहाँ है? जिसे देखने ये सब आये हैं। अरे यार! मेला का देखने वाला, स्वयं ही मेला है। मेला उससे भिन्न नहीं। मैं मेला का अनुभव स्वयं मेला होकर करता हूँ। ऐसे ही जगत् का अनुभव मुझ आत्मा से न भिन्न है और न अभिन्न है। अरे! 'मैं' ही तो हूँ, जो इस रूप में दिख रहा हूँ।
जिसको देखकर भ्रम होता है, वह देखने वाले में तो है नहीं, वह भ्रम तो दिखने में है। चरित्र में भ्रम है, राम में नहीं। जो तीन काल में न हो उसका नाम चरित्र है। तो भासता क्यों है? अरे। यही तो भगवान राम की लीला है।
विकल्प भाव अंदर है, विकल्पाभाव न बाहर है, न भीतर। विकल्पभाव माया है, विकल्पाभाव 'मैं' आत्मा है। देखा हुआ संसार रज्जु में सर्प के समान भासता है। सुना हुआ संसार हूँठ में पिशाच के समान भासता है। अजन्मा संसार बन्ध्यापुत्र के समान और तृष्णा का उपादान संसार मृगजल के समान भासता है। भाव रूप (सत्य) संसार की अनुत्पत्ति है, अभाव रूप (असत्य) संसार की अनुत्पत्ति है और भावाभाव रूप में (सत्य-असत्य दोनों) संसार की अनुत्पत्ति है।
संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व क्या था? सत्य था? असत्य था? या सत्यासत्य था? यदि, कहो सत्य था तो सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जो पैदा होगा वह मरेगा, अतः वह सत्य नहीं। सत्य तो अविनाशी होता है, नित्य होता है। यह संसार नित्य नहीं है, अतः सत्य नहीं। यदि असत्य कहो तो असत्य बन्ध्या का पुत्र होता है। अभाव रूप, जो है ही नहीं वह पैदा क्या होगा। इस तरह भी संसार की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। यदि कहो सत्यासत्य था तो साधक-बाधक पदार्थ साथ-साथ नहीं रह सकते। इस तरह किसी प्रकार से संसार की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती।
डण्डा, यह अपने बनने के पहले क्या था? सत् था या असत् ? सत् कहोगे तो सत् भी कहीं बनता है? सत् तो त्रिकालाबाध्य होता है। असत् कहोगे तो असत् तो बन्ध्या का पुत्र होता है, जो अभाव रूप है, है ही नहीं, परन्तु यह डण्डा तो स्पष्ट दिख रहा है। तब क्या सत्यासत्य है? नहीं, क्योंकि साधक-बाधक पदार्थ एक साथ नहीं रह सकते तब सत्यासत्य भी नहीं। इस तरह डण्डा तीन काल में पैदा नहीं हुआ, न डण्डा है, पर सत्य-सा भासता है। इसकी उत्पत्ति किसी भी तरह सिद्ध नहीं होती। डण्डा यह विकल्प है। अब, जब फोटो लिया जायेगा, तब डण्डा विकल्प का फोटो नहीं आ सकेगा, फोटो उतरेगा उसका जिस पर डण्डे का विकल्प है। अब यह विकल्प किस पर है? उत्तर है- लकड़ी परा लकड़ी यह भी तो विकल्प ही है। लकड़ी, यह विकल्प किस पर है? पृथ्वी पर। पृथ्वी, यह भी तो विकल्प ही है। यह विकल्प किस पर है? (पृथ्वी का आधार जल है) जल पर है। जल, यह विकल्प किस पर है? जल का जो आधार अग्नि है, उस पर। अग्नि, यह विकल्प किस पर है? वायु पर। वायु, यह विकल्प किस पर है? इसका आधार जो आकाश है, उस परा आकाश, यह विकल्प किस पर है? अंत में निर्णय हुआ कि यह विकल्प आधारभूत 'मैं' आत्मा पर हुआ है। तब यह सिद्ध हुआ कि यह डण्डा नहीं है। आधारभूत 'मैं' आत्मा ही है, जिसका फोटो उतरा है। डण्डा, इस विकल्प का फोटो नहीं हो सकता। हाँ, इस विकल्प के अभाव में जो रह गया 'दृश्य' वह डण्डा थोड़े ही है। वह अर्थहीन पदार्थ भास है, जो नारायण है, 'मैं' आत्मा है। प्रश्न है-चित्र, जो उतरा वह अर्थ का है या अर्थहीन भास का? उत्तर है-अर्थहीन भास का। अब इस भास का ज्यों ही तुमने नामकरण किया। (भास यह भी तो नामकरण ही है) विकल्प हो गया। इस तरह जिसका फोटो उतरा है, उसको वाणी व्यक्त नहीं कर सकती, बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती। वह इन्द्रियों से परे का विषय हो गया। अब इस नारायण तत्त्व पर अनन्त विकल्प कर, उन अस्तित्वहीन विकल्पों को सत्य मान लिया गया। बस, यही संसार का रूप है जो अस्तित्वहीन है, है ही नहीं। यदि, प्रपंच है तो प्रपंच के दर्शनकाल में भी उसके अस्तित्व का भान होना चाहिए। परन्तु, उसके दर्शनकाल में प्रपंच न तो स्वदेश में दिखता है और न परदेश में।
स्वरूप के अज्ञान में स्वरूप ही जगत् है और स्वरूप के ज्ञान में जगत ही स्वरूप है। जगत् नहीं भासता, भास ही भासता है।
जिससे सुख और दुःख दोनों का अनुभव हो उसका ही नाम जगत् है और जिससे अनुभव का भी अनुभव न हो, वही 'मैं' भगवान आत्मा हूँ। वस्तु से भय नहीं है, अर्थ से भय है। छोटे मासूम बचे के सामने काला नाग डाल दो, तो वह उसे अर्थहीन स्थिति में देखता है। वह उसे खिलौना समझकर पकड़ने दौड़ता है और पकडना चाहता है। इसका मतलब हुआ कि वह उस पर अर्थ नहीं लगा रहा है। यह काला नाग है, इसके काटने से प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह अर्थ वह नहीं लगाता, इसीलिए वह उससे भय रहित है। इसी तरह सर्वदृश्यमान उसे दिखाई तो पड़ता है, परन्तु अर्थहीन स्थिति में। इस अवस्था में वह भय, घृणा, सुख, दुःख, हर्ष, शोक आदि द्वन्द्वों से रहित रहता है। उसे जो दिखता है, वह वस्तु रूप है अर्थात् 'मैं' आत्मा भार रूप, सत्ता मात्र जो सुख-दुःख से परे है। इसी तरह सर्व दृश्यमान जगत अर्थहीन स्थिति में भास ही भास सत्तामात्र 'मैं' आत्मा राम है, जो विकल्प रहित है, द्वन्द्वों से परे है, पर ज्योंही अर्थ लगाया, विकल्प हुआ कि वहीं से सुख-दुःख, हर्ष-शोक का कारण जगत् प्रपंच का निर्माण हो गया। इस तरह वस्तु 'मैं' आत्मा है और अर्थ जगत प्रपंच है। भगवान आत्मा 'मैं' को कुछ भी मान लेना यही अज्ञान अंधकार का स्वरूप है। इस अज्ञान अंधकार के कारण ही 'मैं' आत्मा भगवान, रज्जु में सर्पवत् संसार प्रपंच तीन काल में नहीं होते हुए भी सत्य-सा भासता है। जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो 'मैं' आत्मा ही हूँ। अरे! रस्सी ही रस्सी है, सर्प था ही नहीं। न अंधेरे में, न प्रकाश में। जिस तरह रज्जु देश में न सर्प की उत्पत्ति है, न विनाश, यह उत्पत्ति आ विनाश तो सर्प देश में है। उसी प्रकार 'मैं' आत्मा भगवान देश में, जगत् प्रपंच न पेट हुआ और न विनाश। 'मैं' आत्मा ही हूँ, सिवाय मुझ आत्मा के कुछ है ही नहीं, त बन्धन और मोक्ष संसार देश का है। आत्म देश में न बन्धन है, न मोक्ष। जब संसार नहीं, तब बन्धन और मोक्ष कहाँ? माताजी को भ्रम चरित्र में हुआ, राम में नहीं।
भंगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती !
एक बात नहिं मोहि सोहानी, जदपि मोह बस कहेहु भवानी ।
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना जेहि श्रुति गाव घरहिं मुनि ध्याना ।।
कहहिं सुनहिं अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिसाच ।
पाषंडी, हरि-पद विमुख, जानहिं झूठ न साच ।।
संसार में जो पाखण्डी, मलिन अन्तःकरण वाले अज्ञानी हैं, उन्हें ही यह होता है, जिनके मन में कुछ, वचन में कुछ और व्यवहार में कुछ इस तरह तीनो भिन्नता होती है, वे ही इस तरह राम को न जानकर, चरित्र को सत्य मानते हैं।
एक राजा था। वह विद्वान, पंडितऔर सन्त महात्माओं से हमेशा यही प्रश्न किया करता था कि महाराज! भगवान पतित पावन है। अतः, वे संसार के सब पापियों को तार देते हैं अर्थात् भवसागर से पार लगा देते हैं। तब, जब सब पुण्यात्मा अपने पुण्य के बल पर स्वर्ग चले जाते हैं और पापियों का उद्धार पतित पावन भगवान कर देते हैं तब नरक तो खाली पड़ा रहता होगा? भगवन्! नरक में कौन जाता है, यह समझाइये। राजा की इस प्रबल युक्ति का जवाब कोई नहीं दे पाते थे।
एक बार उस राजा के यहाँ एक वीतराग महात्मा का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक आदर केसाथ गद्दी पर बिठाया और हमेशा की तरह इनसे भी बड़े गर्व के साथ वही प्रश्न पूछा और कहने लगा कि भगवन्! हमारे धन्य भाग, जो हमें आपके दर्शन हुए। हम बड़े पापी हैं, नीच हैं, सत्कर्म तो कभी जानते नहीं आदि।
उपरोक्त शिष्टाचार के बाद राजा ने इनसे वही प्रश्न पूछा, महात्मा ने राजा के इस प्रश्न और व्यावहारिक शिष्टाचार को सुनते ही उनकी ओर पीठ करदिया और अपना मुँह दूसरी ओर कर कहने लगे। हमसे बड़ी भूल हुई कि ऐसे नीच, पापी, अधर्मी राजा के यहाँ हम आ गये। हमें क्या पता था कि यह ऐसा नीच है। भरी सभा में अपने प्रति महात्मा का यह वचन सुनते ही राजा उद्विग्न हो उठा और कहने लगा- महाराज! आप सन्त महात्मा होकर भी ऐसे अपशब्द अपने मुँह से निकालते हैं। आपको भरी सभा में हमारा इस तरह अपमान करना शोभा नहीं देता। राजा की ऐसी बातें सुनकर महात्मा कहने लगे: अरे! तेरे नीच, अधर्मी, पापी होने की बात तो हमने तुमसे ही सुनी और जानी। इसके पहले तो हम कुछ नहीं जानते थे तो क्या तू पापी, अधर्मी और नीच नहीं है। अभी-अभी तो तू ही अपने मुँह से यह सब कह रहा था, उसी को हमने दुहराया है। अब, जब तुम क्रुद्ध हो तब यह निश्चय होता है कि तेरे मन में कुछ, वचन में कुछ और कर्म में कुछ और ही रहता है। इस तरह वाणी में दम्भ, मन में कपट और कर्म में पाखण्ड का होना पाखंडियों के लक्षण हैं। तो भैय्या ! सुनो, पापियों को तो भगवान तार देते हैं, पुण्यात्मा तो स्वर्ग चले जाते हैं और तेरे जैसे पाखण्डी जिनके मन, वचन और कर्म एक से नहीं रहते वे ही नरक जाते हैं। नरक तुम्हारे जैसे के लिए है, वह खाली नहीं पड़ा रहता। ऐसा कह वे महात्मा उठकर अन्यन्त्र चले गये।
अग्य, अकोविद, अंध अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी ।
लंपट, कपटी, कुटिल, बिसेषी । सपनेहुँ संत सभा नहिं देखी ।।
कहहिं ते वेद असंमत बानी। जिन्ह के सूझ लाभ नहिं हानी ॥
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखहिं किमि दीना ।।
जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका। जल्पहिं कल्पित बचन अनेका।
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं । तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं ॥
बातुल भूत बिबस, मतवारे । ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे ।
जिन्ह कृत महामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा, करिअ नहीं काना।
सोरठा-
अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु राम पद ।
सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम ।।
सगुनहिं अगुनहिं नहिं कुछ भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध बेदा ।।
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥
जो गुन रहित सगुन सोई कैसे। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसे।
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ।।
सन्त महात्मा जन, सगुण और निर्गुण का भेद नहीं मानते। इस रामचरित मानस की यही विशेषता है कि इसमें सगुण-निर्गुण के भेद का कहीं पर उल्लेख नहीं है। सगुण और निर्गुण तो उसके उपासकों की धारणा का नाम है। सन्त तुलसी, भगवान के उपासक थे, सगुण और निर्गुण के नहीं। सगुण को सगुण नहीं मानना, यही निर्गुण भक्ति है। सगुण और निर्गुण ये दोनों भाव उपासक देश में हैं, भगवान देश में नहीं।
स्थूल बुद्धि सगुण मानती है और सूक्ष्म बुद्धि निर्गुण मानती है। ये दोनों बुद्धि जिसकी नहीं है, वह भगवान 'मैं' आत्मा को जानती है (बुद्धि रहित अवस्था) बिन बोध के न सगुण रूप में निष्ठा हो सकती है और न निर्गुण रूप में ही। इन रूपों में तथ चरित्र और लीला में रत तो ज्ञान के बाद ही होता है। अज्ञानी क्या जानेगा कि क्या सगुण है और क्या निर्गुण है। देखकर जाना जाता है और सुनकर माना जाता है। अपने स्वरूप आत्मा को जहाँ देख लेता है, तभी उसमें प्रीति होती है।
देखि चरित, महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरि ।
माना जाता है मन से और जाना जाता है आत्मा से। देखो-विवाह के प्रसंग में जनकपुर में चारों भाइयों के जब सब कार्य सम्पन्न हो चुके, तब बिदाई के समय सबसे भेंट करते हुए, जनक जी सबसे अन्त में राम के पास आते हैं और वे उनसे क्या कहते हैं, वे पहले व्यापक ब्रह्म, सनातन तत्त्व निर्गुण से उठाते हैं, विदेह मुक्त राजा जनक कहते हैं -
राम करौं केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस हंसा ।।
करहिं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता मदु त्यागी ।।
ब्यापकु ब्रह्म अलखु अबिनासी । चिदानंदु निरगुन गुनरासी ॥
मन समेत जेहि जानन बानी। तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ।।
महिमा निगमु नेति कहि कहई। जो तिहुँ काल एक रस रहई ।।
ये व्यापक निराकार का वर्णन हुआ, जिसका भाव यह है -
सन्त का सम्बन्ध हृदय से होता है, बाहर से नहीं। जो हृदय वासना से रहित होता है, उसे मान सरोवर कहते हैं, ऐसे हृदय-रूप मान सरोवर में भगवान राम हंस का निवास होता है।
मुनि महेस मन मानस हंसा ।।
जो व्यापक होता है, वह अलख होता है और जो अलख होता है, वह अविनाशी होता है। सन्त महात्मा जन जिसमें रमते हैं, इसलिए राम सारे चराचर में रम रहे हैं, इसलिए राम सबमें व्यापक हैं, किस तरह? भिन्न होकर, अभिन्न होकर या भिन्ना- भिन्न होकर। यदि भिन्न होकर व्यापेगा तो भिन्न पदार्थ किसके आधार पर रहेगा? अभिन्न होकर कहोगे तो अभिन्न होने से वह एक ही हुआ तो एक में व्यापना कैसे होगा? तो व्यापक केवल कहने मात्र को है, वह जब स्वयं वही है, तब व्याप्य और व्यापक कहाँ हैं? अरे, लकड़ी जब स्वयं ही डण्डा है, तब वह व्यापेगी किसमें? यह दृष्टिगम्य, वाणीगम्य नहीं है, बल्कि अनुभव गम्य है। यह व्यापकपना कैसे है, जैसे वस्त्र में धागा। वस्त्र की मान्यता में, धागा व्यापक है और जब वस्त्र है ही नहीं, केवल धागा ही धागा है तब वह व्यापेगा किसमें?
भाव और अभाव, दोनों के अभाव के भाव में लखना कहाँ रहा? न दृश्य है, न द्रष्टा है, तब लखना कहाँ? न विषय रहे, न इनकी इन्द्रियाँ तब लखना कहाँ है? इसलिए, हे राम! तुम अलख हो।
तुम अजन्मा होने के नाते अविनाशी हो। तुम भासते हो, प्रतीयमान हो, इसलिए चिदानन्द हो और 'है' हो, अस्तित्व हो, इसलिए अलख हो। तीनों गुणों से परे हो इसलिए निर्गुण हो और सर्वगुणों के भण्डार हो, आधार हो, इसलिए गुणराशि हो 'व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानन्द निर्गुण गुणराशी' का यही भाव है।
मन समेत जेहि जान न बानी, तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ।।
तुम मन वाणी के विषय नहीं हो, न तो मन तुम्हें जान सकता और न वाणी तुम्हे कह सकती है। तुम्हारे संबंध में किसी प्रकार का तर्क नहीं किया जा सकता, वेद शास्त्र, पुराण, निगम, आगम सबों ने केवल अपना-अपना अनुमान ही बताया है। जो कहता है कि मैं जानता हूँ, वह जानता नहीं और जो जानता है, वह कहता नहीं।
जो कहता है "मैं भगवान को देखा हूँ, जानता हूँ" वह उसे उससे भिन्न होकर जाना या अभिन्न होकर जाना अथवा भिन्नाभिन्न होकर जाना, किस प्रकार जाना? जानने वाला तो जानकर वही हो जायेगा, गल जायेगा, तब कहेगा कौन? बतायेगा कौन? क्योंकि -
जानत तुम्हहि, तुम्हइ होइ जाइ ।।
उसे जानने वाला तो वही हो गया, बताने वाला रहा नहीं।
जैसे पुतली लौन की सिन्धु थाह गई लैन ।
गलत-गलत वह गल गई, कही न पाई बैन ।
जो गल जायेगा, वह क्या बतायेगा? जब जो जानेगा वह बता नहीं सकता और जो कहता है, मैं जानता हूँ, देखा हूँ, वह देखा नहीं। जितने कहने वाले वाणी-रूप वेद, शास्त्र, निगम, पुराण आदि हैं, उन सबों ने "न इति, न इति" ही कहा।
महिमा निगमु नेति कहि कहई। जो तिहुँ काल एकरस रहई ।।
तुम तीनों काल और तीनों अवस्था में हमेशा एक रस हो, जो 'मैं' जाग्रत में, वही 'मैं' स्वप्न में और वही 'मैं' सुषुप्ति में। जनक जी कह रहे हैं कि हे राम ! ऐसे जो आप हैं, सो मेरी आँखों के सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं।
दोहा-
नयन विषय मो कहुँ भयउ, सो समस्त सुख मूल ।
सबइ लाभु जग जीव कहूँ, भएँ ईसु अनुकूल ।।
देखो, साकार सगुण ब्रह्म में लाकर विलीन कर दिया, मिला दिया। तो भैय्या! सन्त तुलसी की दृष्टि में, सगुण और निर्गुण दो नहीं, एक ही है।
भगवान यदि सचमुच सगुण होते तो संसार भरके सभी उसके उपासक, उस सगुण ही मानते, मगर ऐसा नहीं है। भगवान तो उसे कहते हैं, जिसे संसार भर के सभी पन्थ, मजहब, सम्प्रदाय, सोसायटी, वर्ण और आश्रम भगवान कहें, जो निर्विरो हो, उसके विरोधी कोई भी न हो, जिसे सब की मान्यता प्रदान हो, जो सार्वभौम हो और सर्वमान्य हो, जिससे भिन्न कुछ भी नहीं और जिसके बिना कुछ भी न हो, वह है भगवान। भगवान में कोई विवाद नहीं है, जब सर्व का भगवान एक ही है, तब मेरा भगवान, तेरा भगवान, सगुण भगवान, निर्गुण भगवान आदि भेद कहाँ रहा? भगवान माने भगवान जानकर, ज़ो भगवान की उपासना करते हैं, वही सच्चे उपासक हैं और भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, ऐसा मानकर जो उपासना करते हैं, वे भगवान के उपासक नहीं, माया (मान्यता) के ही उपासक हैं। प्रश्न-भगवान माने भगवान जानना क्या है और भगवान माने भगवान मानना क्या है?
अपने स्वरूप 'मैं' आत्मा के माने 'मैं' आत्मा जानोगे, तब तुमको यह अर्थ लगेगा कि भगवान माने भगवान है और अपने स्वरूप 'मैं' आत्मा को कुछ भी मानोगे, तब यही अमुक भाव मान्यता है, इसमें भगवान माने भगवान मानना है, क्योंकि ज्यों ही कुछ माना कि 'मैं' से अलग हुआ। एक बार हमसे किसी सज्जन ने पूछा स्वामी जी! मैं सगुण भगवान को भजूँ या निर्गुण भगवान को? हमने कहा भैय्या! तुम, न तो सगुण भगवान को भजो और न निर्गुण भगवान को भजो, इस झगड़े में क्यों पड़ते हो, तुम सीधे भगवान को भजो। देखो, राम सत् स्वरूप है, चित् स्वरूप है और आनन्दस्वरूप है।
अयोध्या के महाराज दशरथ के जब चार पुत्र हुए, तब उनने अपने सूर्यवंश के कुल गुरु वशिष्ट को बुलाकर उनकी विधिवत् पूजा की और तदोपरान्त, इन चारों भाइयों के नामकरण करने के लिए उनसे विनती की, गुरु वशिष्ठ जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से हैं तथा त्रिकालदर्शी ब्रह्म निष्ठ महात्मा हैं, उन्होंने ज्योतिष और पंचांग देखकर चारों भाइयों का नामकरण किया।
भगवान राम के नाम के संबंध में 'राम' यह नाम उन्होंने क्यों रखा, उस पर मानसकार कहते हैं कि -
जो आनंद सिन्धु सुखरासी । सीकर तें त्रैलोक सुपासी ।।
सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा ।।
जो आनन्द के समुद्र है और सीकर अर्थात् बालू के एक कण से लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक के लिए जो सुपास हैं अर्थात् विश्राम स्थल हैं, वहीं पहुँचने के बाद ही सबको फुर्सत मिलती है, विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए इनका नाम 'राम' रखा।
अनादि काल से जीव मात्र की यात्रा, आनन्द के लिए है, कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी दुःख नहीं पाना चाहता। मैं सदा सुखी रहूँ, यही सबकी चाह है, तब आनन्द तो जीव मात्र को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन विषयों में रात-दिन मिलता ही रहता है, तब जीव की आनन्द यात्रा समाप्त हो जाना चाहिए, परन्तु यात्रा की समाप्ति क्यों नहीं होती?
उत्तर है-उसका प्रयास आनन्द सिन्धु के लिए है, आनन्द सागर के लिए है, न कि आनन्द की डबरी, आनन्द का तालाब, आनन्द का सरोवर। विषयानन्द जो है, वह आनन्द की डबरी है, तलैय्या है, सरोवर है जो कीचड़युक्त है, क्षणिक है, अनित्य है, आगमापायी है। जीव की यात्रा तो आनन्द सागर के लिए है, नित्यानन्द, पूर्णानन्द, परमानन्द, निजानन्द, आत्मानन्द के लिए है। तब "आनन्द सिन्धु सुखरासी" तो भगवान राम ही है, इसलिए जीव की यात्रा भगवान राम की प्राप्ति के लिए है, जब तक उसे उसकी प्राप्ति न हो जायेगी, तब तक उसकी यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। चाहे इसके लिए उसको कितनी ही बार जन्म लेना पड़े। तब तक यह यात्रा रहेगी, विश्राम नहीं पा सकता, उसे शांति नहीं मिल सकती।
वह सुख, सुख नहीं, जिसमें दुःख है, डर है, रोना है।
मिलावट से जो है खाली, उसी का नाम सोना है ।।
करो तुम चूर्ण हीरे को, मगर काला नहीं होता ।
अरुण पर फेंक दो तुम धूल, अंधियारा नहीं होता ।।
स्त्री सुख, पुत्र सुख, सम्पत्ति सुख, यौवन सुख, कीर्ति सुख आदि जितने भी सुख हैं उनमें दुःख है, डर है और रोना है। स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, कीर्ति इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इनकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तब कहीं इनकी प्राप्ति हो पाती है और ये कुछ काल तक रह पाते हैं, इनमें यही दुःख है। स्त्री पुत्र न मर जायें, कीर्ति और सम्पत्ति नष्ट न हो जाय, धन को चोर न चुरा ले, लुट न जाय, इनका भय नित्य बना रहता है। इनमें यही डर है। इनके नाश हो जाने पर असहनीय दुःख के साथ, रोना पड़ता है, यही इनमें रोना है। इसलिए, ये सब सुख, सुख नहीं है, क्योंकि इनमें दुःख है, डर है, रोना है ये अनित्य सुख है। जिसको नित्य सुख, परम सुख, परमानन्द, सहजानन्द, नित्यानन्द कहते हैं, वह सारे चराचर का अस्तित्व, भगवान आत्मा 'मैं' है। उसको चाहे राम कह लो, कृष्ण कह लो जो तुम्हारी मर्जी आवे कहो। इस नित्य सुख की प्राप्ति के बिना, विश्राम नहीं मिल सकता। मानसकार कहते हैं।
सरिता जल, जल निधि महुँ जाई, होइ अचल, जिमि जिव हरि पाई ।।
नदी बहते-बहते जब तक समुद्र में नहीं पहुँच जाती, तब तक उसे विश्राम नहीं मिल सकता। वह अनेकों पहाड़, जंगल, चट्टान आदि से टकराती हुई, धक्का खाती हुई, चलती रहती है, परन्तु ज्यों ही वह समुद्र में पहुँची कि उसे विश्राम मिल गया, उसका बहना बन्द हो गया, उसका उछलना कूदना हमेशा के लिए बंद हो गया, उसकी यात्रा समाप्त हो गयी, वह शांत हो गयी। बस, इसी तरह जीव की दशा है, जब तक वह 'हरि' (जो दुख को हरे, उसको हरि कहते हैं) अर्थात् भगवान को न पा लेगा, तब तक वह अचल नहीं हो सकता। उसका चलना बन्द नहीं हो सकता, आवागमन लगा ही रहेगा। ज्यों ही उसे 'आनन्द सिन्धु सुखरासी' भगवान राम 'मैं' आत्मा की प्राप्ति हुई कि वह विश्राम पा गया, अचल हो गया, आवागमन के चक्र से छूट गया। उसका भटकना बन्द हो गया।
राम के लक्षण हैं – जिसे पाकर, जीव, आवागमन से फुरसत पा जाता है।
अखिल लोक दायक विश्रामा ।।
जो सुख के धाम हैं "सुखधामा"
जो सारे चराचर के सुपास है -
सीकर ते त्रैलोक सुपासी ।।
जो सत् होते हुए चित् है, चित् होते हुए, आनन्द स्वरूप है। अर्थात् सच्चिादनन्द स्वरूप राम है।
राम सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर ।
अबिगत अकथ अपार नेति-नेति नित निगम कह ।।
राम का जो स्वरूप है, वह मन वाणी का विषय नहीं है, वह अविनाशी, असीम और अनन्त है। वेद शास्त्र, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, पता लगाते-लगाते जब स्वयं डूबने लगती हैं, तब न इति, न इति कहते हुए, वहाँ से भाग जाती हैं।
अवस्थाओं का प्रपंच काल के साथ परिवर्तन होते रहता है। जगत् प्रपंच, काल का सहचारी है। काल की गति कैसी अव्याहत है कि सर-सर-सर-सर-सर-सर चला जा रहा है। इसके सामने राकेट की भी कोई हस्ती नहीं है। प्रतिपल वर्तमान, भूत होते जा रहा है और भविष्य, वर्तमान होते जा रहा है। सर्वकाल मुझमें समाते चले जा रहे हैं। 'मैं' काल का भक्षण करते चला जा रहा हूँ।
जो कालहु कर काल भयंकर, बरनत उमा सारदा संकर।
प्रपंच और काल दोनों की आखिरी मंजिल 'मैं' आत्मा हूँ। तीनों अवस्था और तीनों काल के परिवर्तन काल में सर्व के परिवर्तनपने में 'मैं' नित्य एकरस रहा, अपरिवर्तनशील रहा। जो 'मैं' भूत में, वही 'मैं' वर्तमान और भविष्य में और जो 'मैं' जागृत अवस्था में वही 'मैं' स्वप्न और सुषुप्ति में, वही 'मैं' मूर्च्छा में। अस्पताल में जब किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है, तो डॉक्टर पहले उसे मूर्च्छित कर देता है, तब बेहोशी की हालत में उसके शरीर के अंगों की चीरा-फाड़ी करता है। ऑपरेशन समाप्त होने पर जब वह आदमी होश में आता है, तब कहता है कि भैय्या! मेरा बड़ा खतरनाक ऑपरेशन हुआ, मैं तीन घंटे तक ऐसा बेहोश रहा कि कुछ पता ही नहीं चला।
अब विचार करना है कि यदि 'मैं' आत्मा सचमुच बेहोश हो गया होता, तो यह कौन बताता कि अरे यार! मैं तीन-तीन घंटे तक बेहोश रहा। इस तीन घंटे की बेहोशी का कौन अनुभव करता है? कुछ पता ही नहीं चला, इस 'नहीं पता' का पता, कैसे लगता? मतलब यह कि 'मैं' बेहोश नहीं हुआ 'मैं' ज्यों का त्यों रहा।
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म
जानना ही तो मुझ आत्मा का स्वरूप है। प्रक्रिया समझो - देखो भैय्या! पहिले इन दो शब्दों को ठीक-ठीक समझ लो 'मैं' और 'मेरा'।
'मैं' का अर्थ मेरा नहीं होता, और 'मेरा' का अर्थ 'मैं' नहीं होता। यदि मेरा का अर्थ 'मैं' होता, तो मेरा मकान कहने से 'मैं' मकान हो जाता, मेरी साइकिल कहने से 'मैं' साइकिल हो जाता, परन्तु ऐसा नहीं होता। 'मैं' कर्तृवाचक शब्द है, यह (मैं) खुद के लिए कहा जाता है और मेरा सम्बन्ध सूचक शब्द है, अर्थात् जो चीज अपनी होती है, जिस चीज से अपना सम्बन्ध होता है, उसके लिए मेरा कहा जाता है। जैसे मेरा मकान, मेरी साइकिल, मेरी पुस्तक, मेरी गाडी, मेरा बैल आदि। इसका अर्थ 'मैं' मकान, 'मैं' साइकिल, 'मैं' पुस्तक, 'मैं' गाडी और 'मैं' बैल नहीं हो जाता। ये सब मेरे हैं, इसलिए इनके लिए 'मैं' मेरा कहा करता हूँ। 'मैं' इन्हें मेरा कहने वाला, इनसे सर्वथा अलग हूँ। इसी तरह 'मैं' मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरे कान, मेरी आँख और अन्त में मेरा शरीर आदि कहा करता हूँ। इसका अर्थ हुआ कि 'मैं' सिर नहीं, 'मैं' हाथ नहीं, पैर, कान, आँख, नाक, मुँह और शरीर नहीं, क्योंकि इन सबको 'मैं' मेरा कह रहा हूँ। अतः 'मैं' इन्हें मेरा कहने वाला इनसे अलग हूँ। जब शरीर में नहीं तब, इस शरीर को ही लोग रामदत्त, शिवदत्त, गणेशदत्त, मोहनलाल, रामलाल कहते हैं। मैं रामदत्त, शिवदत्त, गणेशदत्त आदि नहीं हूँ, क्योंकि यदि 'मैं' रामदत्त, शिवदत्त होता, तो मेरे पैदा होते ही लोग पुकार उठते कि अरे भाई ! दौड़ो रामदत्त पैदा हो गया, शिवदत्त पैदा हो गया, परन्तु ऐसा किसी ने नहीं कहा, शरीर के पैदा होने के बाद व्यवहारिक जगत् में काम चलाने के लिए शरीर का ही नामकरण कर लिया जाता है। अतः, शरीर का ही नाम रामदत्त, शिवदत्त आदि है। तब शरीर ही रामदत्त, शिवदत्त है, 'मैं' शरीर नहीं हूँ। अतः मैं रामदत्त, शिवदत्त नहीं हूँ। जब 'मैं' शरीर नहीं हूँ तब शरीर के जितने विकार हैं वे सब विकार भी मुझमें नहीं हैं यथा शरीर ही छोटा, बड़ा, बालक, युवा, वृद्ध होता है।'मैं' उससे अलग होने के कारण न छोटा हूँ, न बडा हूँ, न बालक हूँ, न युवा हूँ, न वृद्ध हूँ।
काला, गोरा, अन्धा, लूला, लंगड़ा आदि शरीर होता है, 'मैं' नहीं। स्त्री और पुरुष शरीर होता है, 'मैं' न स्त्री हूँ, न पुरुष। ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र आदि शरीर है, 'मैं' नहीं। गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, संन्यासी, शरीर होता है, 'मैं' नहीं। पिता, पुत्र, मामा, काका, भाई, भतीजा आदि शरीर को ही कहते हैं। इस शरीर से अलग होने के नाते, मैं ये सब नहीं हूँ। निरालम्बोपनिषत् में है -
न चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिनः ।
न जातिरात्मनो जातिर्व्यवहार प्रकल्पिता ।।
जिसका भाव है कि न तो चमड़े की कोई जाति होती है, न रक्त की जाति होती है, न माँस की कोई जाति होती है, न हड्डी की जाति होती है और न आत्मा की ही कोई जाति होती है। यह तो केवल संसार में व्यवहार चलाने के लिए जाति की कल्पना कर ली गयी है।
यह शरीर ही जन्मता और मरता है 'मैं' इससे अलग हूँ, अतः न 'मैं' जन्मता हूँ, न मरता हूँ।
अब देखो -
शरीर बदलते रहता है, 'मैं' इनसे अलग होने के कारण इसके बदलने के साथ- साथ 'मैं' नहीं बदलता।
जैसे-वृद्धावस्था में बचपन का कोई मेरा दोस्त या मित्र जब मुझसे मिलता है, तब मैं उनका परिचय दूसरों को इस प्रकार देता हूँ। भाई! ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैं इनके साथ प्रायमरी पढा हूँ, ये मेरे युवावस्था के दोस्त हैं, इनके साथ मैं कॉलेज पढा हूँ। अब वह प्रायमरी पढने वाला बालक शरीर नहीं रहा बदलकर युवा हुआ और कॉलेज पढ़ने वाला, वह युवा शरीर भी नहीं रहा, बदलकर वृद्ध हुआ। परन्तु, जो 'मैं' प्रायमरी पढने वाला शरीर में था, वही मैं युवावस्था में कॉलेज पढ़ने वाला शरीर में भी रहा। अब वह बालक शरीर नहीं रहा, बदलकर युवा हुआ, वह युवा शरीर भी नहीं रहा, बदलकर वृद्ध हो गया। परन्तु, जो 'मैं' बालक शरीर में था, वही 'मैं' युवा शरीर में रहा और जो 'मैं' बालक और युवा शरीर में रहा वही 'मैं' अब इस वृद्ध शरीर में भी हूँ।
वह 'मैं' तीनों शरीर में सदा एक रस, एक-सा रहा। शरीर बदल गये, परन्तु 'मैं' नहीं बदला, क्योंकि यदि शरीर के बदलने के साथ-साथ 'मैं' भी बदल गया होता तो यह कौन बताता, यह ज्ञान किसे रहता कि 'मैं' इनके साथ प्रायमरी पढा था, इनके साथ कॉलेज पढ़ा था आदि। इससे सिद्ध हुआ कि शरीर तो बदला, पर 'मैं' इन सब शरीरों में सदा एक रस, एक-सा रहा। इस तरह शरीर के सम्पूर्ण विकारों से 'मैं' अलग हूँ। मुझमें ये विकार नहीं है। मैं, मेरा मकान कहता हूँ, इसका अर्थ 'मैं' मकान नहीं हूँ। मकान में रहता हूँ, इसलिए मैं इसे मेरा कह लिया करता हूँ। इसी तरह इस शरीर में 'मैं' रहता हूँ। अतः मेरा शरीर कहता हूँ।
जैसे-मकान, मिट्टी, ईंटा, गारा आदि से बनाकर लकड़ी खम्भे, काँड, बल्ली आदि लगाकर मिट्टी, सीमेंट आदि से उसकी छबाई करके चूना, गेरु, नीला थोथा आदि से उसकी पुताई की जाती है, इसी तरह यह शरीर हड्डी, पसली आदि खम्भे और काँड बल्ली से खड़ा किया गया, चमड़े से इसकी छबाई हुई है, नौ द्वार (दो कान, दो आँख, दो नाक, एक मुँह, मल और मूत्र त्याग करने की दो इन्द्रियाँ) इसके दरवाजे और खिड़कियाँ हैं। किसी का शरीर काला है, किसी का गोरा, किसी का साँवला। यह चूना, गेरू और नीला थोथा से पुताई करने के समान है। इस तरह 'मैं' के रहने का यह शरीर मकान है।
'मैं' मकान में रहता हूँ, अतः इसे 'मैं' मेरा कह लिया करता हूँ, परन्तु वास्तव में यह मकान भी मेरा नहीं है, क्योंकि यह मिट्टी, ईंट, गारा आदि से बना है। अतः यह ईंट, गारा, मिट्टी आदि का मकान है, मेरा नहीं। इसी तरह, यह शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से बना हुआ होने के कारण यह पंच महाभूतों का है, मेरा नहीं।
छिति जल पावक गगन समीरा ।
पंच रचित अति अधम सरीरा ।।
इसके अंदर 'मैं' हूँ जरूर, पर यह 'मैं' नहीं हूँ। यह हुआ स्थूल शरीर। परमात्मा और अपने आप में भेद का जो भ्रम है, यह सब देहाध्यास के कारण है। जब तक साढ़े तीन हाथ की खुदी है, तब तक खुदा दूर है और जब यह देहाध्यास गया तब फिर खुदा ही खुदा है। खूब समझ लो, यह शरीर उत्पत्ति, विनाश वाला है, घटने-बढ़ने वाला है, इसको संघात कहते हैं, नाशवान कहते हैं।
देहात्मबुद्धिजं पापं न पद् गोबध कोटिभिः ।
आत्माऽहं बुद्धिजं पुण्यं, न भूतं न भविष्यति ।।
(उपनिषद)
यदि शास्त्रों पर विश्वास है, तो अपने आपको जो देह मानता है उसे एक करोड़ गौ की हत्या का पाप लगता है और जो अपने आपको आत्मा 'मैं' हूँ ऐसा जानता है, इससे अधिक पुण्य भी नहीं होता। इसलिए जान लो कि यह स्थूल शरीर न 'मैं' हूँ और न यह मेरा है। इस तरह, यह सिद्ध हुआ कि न 'मैं' शरीर हूँ, न मेरा शरीर है।
अब आगे समझो -
मैं बुद्धि के लिए कहता हूँ, मेरी बुद्धि इस बात को नहीं समझ रही है। मैं चित्त के लिए कहता हूँ, मेरा चित्त इस काम में नहीं लग रहा है।
मैं मन के लिए कहता हूँ, मेरा मन जरा दूसरी ओर चला गया था, आपने क्या कहा मैं समझा नहीं, जरा फिर से कहिए। मैं, प्राण के लिए कहता हूँ कि मेरे प्राण भूख से व्याकुल हो रहे हैं आदि। इस तरह मैं कहता हूँ, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरे प्राण आदि। जिसका अर्थ हुआ कि 'मैं' बुद्धि, चित्त, मन, प्राण आदि नहीं हूँ, क्योंकि इन सबों को 'मैं' मेरा कह रहा हूँ। अतः, 'मैं' इन्हें मेरा कहने वाला इन सबों से सर्वथा अलग हूँ। इनसे भी भिन्न हूँ, मैं इन सब को जानता हूँ, ये सब मेरे दृश्य हैं, 'मैं' इनका द्रष्टा हूँ।
स्वर्ण यथां ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तद्भिज्ञ आप्नुयात् ।
क्षेत्रेषु देहेषु तथाऽऽत्म योगैरध्यात्मवित् ब्रह्मगतिर्लभेत ।।
अर्थात् हेमकार यानी सोनार, सोने को गलाकर खोट भाग को त्याग कर स्वर्ण का खरा भाग ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जहाँ तक मेरा कहा जाता है अथवा जिस पदार्थ के लिए मेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह सब खोट है और त्याज्य है। शेष जो 'मैं' रह जाता है, वही स्वर्ण के समान खरा अपना आप 'मैं' नाम से प्रसिद्ध भगवान आत्मा सर्व का सर्व है, क्योंकि 'मैं' में कोई धोखा नहीं, बाकी सब में धोखा है, इसलिए उपनिषत् की भाषा में श्रुति 'मैं' आत्मा को प्रत्ययसार कहती है। प्रत्ययसार का अर्थ होता है 'विश्वास पात्र'।
अब यह निश्चय हुआ कि जो 'मैं' इन सबों स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त, प्राण आदि सबसे भिन्न, सबका जानने वाला वह 'मैं' कैसा हूँ? कौन हूँ? ऐसा 'मैं' आत्मा, सत्, चित्त, आनन्द स्वरूप हूँ।
सत्- (सत्य) उसे कहते हैं, जिसका तीनों काल और तीनों अवस्थाओं में, कभी भी अभाव न हो। सदा एक रस नित्य रहे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएँ और भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीन काल हैं।
देखो-इन तीनों अवस्थाओं और तीनों काल में 'मैं' का कभी भी अभाव नहीं होता। 'मैं' सदा एक रस विद्यमान रहता है।
समझो -मैं सुबह पाँच बजे सोकर उठता हूँ, तब 'मैं' रहता हूँ, तभी तो पांच बजे को जानता हूँ, फिर छः बजे, इसे भी मैंने जाना, फिर सात बजे, आठ बजे, नौ, दस, ग्यारह, बारह, एक, दो बजते हुए रात के दस बज गये, इन सबको 'मैं' जानते गया। इस तरह पाँच बजे सुबह से लेकर दस बजे रात्रि तक का सब समय जाग्रत अवस्था कहलाती है, इसके सारे प्रपंचों को मैंने जाना। अतः इन सारे प्रपंचों के जानने वाले 'मैं' का अभाव नहीं रहा। यथा-पाँच बजे सुबह से लेकर दस बजे रात्रि तक का काल (समय) कहाँ चला गया, काल अर्थात् समय वे सब अब नहीं रहे, परन्तु 'मैं' एक रस रहा। वे सब समय (काल) कहाँ गये।
अरे! "मैं" ने उन्हें खा लिया "मैं" ने उनका भक्षण कर लिया।
जो कालहु कर काल भयंकर ।
वरनत उमा सारदा संकर ।।
अतः, मैं आत्मा कालों का भक्षण करने वाला कालों का भी महाकाल सिद्ध हुआ।
दस बजे रात्रि में सोने के बाद रात्रि में स्वप्न हुआ, तब इन स्वप्न के सब प्रपंचो को जाग्रत अवस्था के समान ही मैंने अनुभव किया। उन्हें देखा, जाना। तभी तो सोकर उठने पर अपना स्वप्न का अनुभव दूसरों से व्यक्त करता हूँ। कहता हूँ कि आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा, यदि उस स्वप्न अवस्था में 'मैं' नहीं रहता, मेरा अभाव होता तो अपना यह अनुभव कि मैंने आज ऐसा स्वप्न देखा, इसे कौन बताता? इससे सिद्ध हुआ कि स्वप्न में भी 'मैं' नित्य विद्यमान रहा, मेरा अभाव नहीं रहा।
तीसरी अवस्था सुषुप्ति (गाढी नींद) है। गाढी नींद से जब मैं सोकर उठता हूँ तब कहता हूँ कि अहा! आज मैं ऐसी सुख की नींद सोया कि कुछ पता ही नहीं रहा, बड़ा आनन्द आया। अब विचार करना है कि इस गाढी नींद में 'मैं' सोया नहीं, सोना जागना मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। यदि, 'मैं' सो गया होता, तो गाढी नींद के आनन्द का अनुभव कौन करता? "कुछ पता ही नहीं रहा" इस पता का पता, कौन जानता ? मैं इस गाढ़ी नींद में भी नित्य रहा, तभी "बड़ा आनन्द आया" और "कुछ पता ही नहीं रहा" इन दोनों का अनुभव किया। अतः, सिद्ध हुआ कि सुषुप्ति अवस्था में भी मेरा अभाव नहीं रहा, 'मैं' विद्यमान रहा। इस तरह जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का 'मैं' द्रष्टा, साक्षी और अनुभव करने वाला हूँ।
काल तीन होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। अभी जो समय बीत रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके सारे प्रपंचों को 'मैं' नित्य देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, यह तो प्रत्यक्ष है। जो वर्तमान काल में 'मैं' नित्य हूँ। जो समय बीत चुका उसे भूतकाल कहते हैं, आज के पहिले 'मैं' नहीं था, ऐसा कहना, अपना अनुभव बताना ही है। आज के पहिले 'मैं' नहीं था, इसको नहीं था, वह बता रहा है या जो था, वह बता रहा है? 'था' वही बता रहा है। यदि 'मैं' नहीं रहता तो 'मैं नहीं था' इसका अनुभव कौन करता? इसका अनुभव करने वाला 'मैं' वहाँ मौजूद था, तभी यह अनुभव बता रहा हूँ कि मैं नहीं था। अतः, यह सिद्ध हुआ कि मेरा यह कहना ही कि 'मैं नहीं था' यह सिद्ध करता है कि 'मैं' था। मेरा अभाव भूतकाल में भी नहीं रहा, वहाँ भी 'मैं' था।
एक बार हम रेल में सफर कर रहे थे। दिल्ली के आसपास एक स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, तब हमारी दृष्टि यह कौन-सा स्टेशन है, यह जानने के लिए प्लेटफार्म पर लगे बोर्ड पर गयी। बोर्ड देखा तो मन प्रफुल्लित हो गया। उसमें लिखा था, 'मैं था' अर्थात् उस स्टेशन का नाम था 'मैं था'। इसका रहस्य समझो। यह स्थान (ग्राम या शहर) यह बता रहा है कि जब यहाँ स्टेशन नहीं बना था, तब भी "मैं था" मेरा अभाव नहीं रहा। अभी भी "मैं था" ही हूँ और आगे चलकर यदि स्टेशन नहीं भी रहेगा तब भी "मैं था" ही रहूँगा। वाह! यह लौकिक रहस्यमय घटना है। यह कह रहा है कि मेरे ही समान जब यह शरीर रूप स्टेशन है (वर्तमान) तब "मैं था" हैं। यह शरीर रूप स्टेशन नहीं रहेगा। (भविष्य) तब भी "मैं था" रहूँगा और यह शरीर रूप स्टेशन नहीं बना था (भूतकाल) तब भी "मैं था" ही रहा। मेरा अभाव तीनो काल में कभी नहीं हुआ।
इसी तरह यह कहना कि भविष्य में 'मैं' नहीं रहूँगा, यह भी अपना अनुभव ही बताना है और अपना अनुभव तभी बताया जा सकेगा, जब अनुभव करने वाला वहाँ मौजूद रहेगा। अतः, सिद्ध हुआ कि 'मैं' का अभाव तीनों काल में नहीं हुआ। इस तरह तीनों काल और तीनों अवस्थाओं में 'मैं' नित्य एक रस विद्यमान रहा, अतः 'मैं' सत्य हूँ।
'मैं' आत्मा चेतन हूँ। जो अपने आपको जाने और दूसरों को भी जाने, उसे चेतन कहते हैं। 'मैं' आत्मा अपने को जानता हूँ और अन्य को भी जानता हूँ।
'मैं' हूँ, इसको तो सारा संसार जानता है, कभी भी ऐसा कोई नहीं कहता कि दौडो रे, 'मैं' तो नहीं हूँ। मुझमें 'मैं' नहीं रहा। इससे पता चलता है कि 'मैं' अपने को जानता हूँ, अन्य को भी जानता हूँ, कान के सुनने, न सुनने, आँख के देखने, न देखने, मन के आने-जाने, सुखी-दुःखी होने, चंचलता-स्थिरता आदि को जानता हूँ। चित्त को जानता हूँ, प्राण को जानता हूँ, बुद्धि को जानता हूँ। शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और इनके विषय को जानता हूँ, यह दूसरों को जानना हुआ। तीनों काल और तीनों अवस्थाओं के सारे प्रपंच को जानने के कारण 'मैं' आत्मा चेतन हूँ।
'मैं' आत्मा, आनन्द स्वरूप हूँ। अपने आप 'मैं' आत्मा से किसी को वैराग्य नहीं होता। स्त्री, पुत्र, धन आदि से तथा अपने शरीर, प्राण आदि से भी मनुष्य को वैराग्य हो जाता है अर्थात् जब कभी शरीर बीमार होकर अधिक समय तक जीर्ण अवस्था में असह्य दुःख भोगने लगता है, तब वह अत्यन्त निराश होकर कहता है कि मेरा यह शरीर शीघ्र छूट जाय, मेरे प्राण निकल जायें आदि। तब मैं सुखी हो जाऊँ। इस तरह शरीर और प्राण से भी मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। परन्तु, अपने 'मैं' से एक क्षण भी कभी वैराग्य नहीं होता। वैराग्य तो दुःख से होता है, आनन्द से नहीं। इससे सिद्ध होता है कि 'मैं' आत्मा आनन्द स्वरूप हूँ। इस तरह 'मैं' आत्मा सत् (सत्य) चित् (चेतन) आनन्द रूप, सच्चिदानन्द हूँ। अब इसी को सूत्र रूप में समझो -
1. 'मैं' हूँ इस अस्तित्व में कभी किसी को शंका नहीं होती, अतः 'मैं' आत्मा सत्य हूँ।
2. 'मैं' हूँ इसका किसी को भी अज्ञान नहीं होता, अतः 'मैं' चेतन हूँ।
3. 'मैं' हूँ इससे किसी को भी वैराग्य नहीं होता, अतः 'मैं' आनन्द स्वरूप हूँ।
'मैं' आत्मा शरीर के एक जगह हूँ या शरीर के सब जगह हूँ।
भाई! मैं आत्मा शरीर में नख से लेकर सिर तक सब जगह एक रस, ठसाठस परिपूर्ण हैं।
देखो-जब पैर में काँटा चुभता है, तब मैं उसे जानता हूँ। पेट में, सिर में, आँख, कान, नाक आदि शरीर के किसी भी अंग में, जब कभी भी कुछ सुख-दुःख होता है, स्पर्श होता है तो 'मैं' तुरन्त उसे उसी जगह से ही जानता हूँ। अतः सिद्ध है कि 'मैं' शरीर में सब जगह ठसाठस परिपूर्ण हूँ।
'मैं' आत्मा निराकार हूँ या साकार हूँ? भैय्या! मैं आत्मा न निराकार हूँ, न साकार हूँ। अरे! मैं आत्मा, इन दोनों को जानने वाला, इन दोनों से परे हूँ।
देखो, जब मेरे सिर में दर्द होता है तो वह कितना सूक्ष्म होता है, आँख उसे देख नहीं सकती, हाथ छू नहीं सकता, वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। कितना बडा दर्द है? दर्द का क्या रूप रंग है? ऐसा पूछे जाने पर मैं यही कहता हूँ कि भैय्या! इस दर्द को वही जाने, जिसे दर्द हुआ हो। तब एक तो दर्द सूक्ष्म और उस सूक्ष्म दर्द को देखकर, छूकर बताने वाला 'मैं' आत्मा कितना सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूँ कि इसकी सूक्ष्मता के सामने, आकाश इतना सूक्ष्म होते हुए भी सुमेरू पर्वत के समान स्थूल है। ऐसा 'मैं' आत्मा साकार और निराकार दोनों का जानने वाला इन दोनों से परे हूँ।
इस तरह 'मैं' आत्मा सत्, चित्, आनन्द रूप सच्चिदानन्द भगवान आत्मा ही हूँ, इसका अर्थ शरीर को लेकर मत समझो। अनादि काल से शरीर को 'मैं' मानकर बैठे हो, अतः शरीर से अलग होना ही नहीं चाहते।
अरे यार! इस मल-मूत्र के भाँड, हड्डी, चमडे को भगवान नहीं कहा जा रहा है, यह नाशवान है, अनित्य है। इस शरीर में जो नित्य 'मैं' नाम से बोल रहा है, भगवान आत्मा 'मैं' की व्याख्या हो रही है और हमेशा 'मैं' का अर्थ, इसी तरह शरीर को छोड़कर इसके भीतर का बोलने वाला 'मैं' को समझना चाहिए।
'मैं' को तन मत मानिये, 'मैं' है सर्वाधार । '
मैं' से सिद्धी सर्व की, 'मुक्ता' देखु विचार ॥
आप भुलानो आप में, बन्ध्यो आप में आप ।
जाको ढूँढत फिरत है, सो तू आपै आप ।।
सम्पूर्ण दूध में मक्खन व्यापक रहता है, परन्तु वह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, जब तक वह मथानी से न मथ लिया जाय। मथानी से मथकर ही मक्खन प्राप्त किया जाता है, ऐसे ही सारे चराचर में या सम्पूर्ण शरीर में, पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक 'मैं' आत्मा घनभूत, ठसाठस, लबालब पूर्ण रूप से व्याप्त हूँ, उसे विचार रूपी मथानी से मथकर आत्मा रूपी मक्खन को प्राप्त करना चाहिए। 'मैं' और मेरा का विचार पूर्वक पठन, चिन्तन, मनन ही विचार रूपी मथानी से मथना है जिससे आत्मा रूपी मक्खन की प्राप्ति होती है।
जो सबको जानता है, उसको जान लेना ज्ञान है। जो सबको देखता है, उसका दर्शन, भगवत दर्शन है। जो सबको सुनता है, उसको सुनना भगवन्नाम श्रवण है।
हमीं थे भूले, हमीं में ढूँढ़े, हमीं गई, तो हमीं मिले ।
हमीं ने खोजा, हमीं ने पाया, कमी हुई तो हमीं मिले ।।
मोरे हीरा गवाँ गयेव, कचरा मा ।
कोई पूरब, कोई पश्चिम बतावै, कोई पानी कोई पथरे मा ।।
जोगी, पैगम्बर, पीर, अवलिया, सभी भुलानो नखरे मा ।। 1।।
मथुरा ढूँढेव, वृन्दावन ढूँढ़ेव, ढूँढ़ेव कोठरिया के अंतरे मा ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, पायेवँ मैं अपने अंतर मा ।।2।।
मोरे हीरा गवाँ गयेव, कचरे मा ।।
मनुवा अब हँस ले दिल खोल, तूने पाया लाल अमोल ।
सत् चित्, आनन्द तू तो निकला बजा खुशी के ढोल ।।
मनुवा ।। जब सत वाक्य सुने सद्गुरु के, खुल गई जग की पोल ।
जी चाहे तो बोल किसी से, जी चाहे मत बोल ।। ।। मनुवा।।
एक बार राम दरबार लगा हुआ था, तब दरबार में भगवान राम ने हनुमान जी पूछा कि हनुमान! तुम कौन हो? इस प्रश्न के होते ही हनुमान जी सरकारी प्रश समझ सतर्क हो बड़ी सावधानी से हाथ जोड़कर सभा के मध्य में खड़े हुए और बड़ नम्रता से बोले - भगवन् !
देहदृष्टया तु दासोऽहं, जीवदृष्टया त्वदंशकः ।
वस्तुतस्तु त्वमेवाहं, इति मे निश्चितामतिः ।।
देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीवदृष्टि से मैं आपका अंश हूँ और प्रभो! यदि सचाई से पूछो, वास्तव में कहो तो जो आप हैं वही 'मैं' हूँ। ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है।
परमात्मा के दो लक्षण हैं -
1. तटस्थ लक्षण,
2. स्वरूप लक्षण
1. जो लक्षण 'मैं' के अस्तित्व का प्रतिपादन करे, उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। ब्रह्म की जो व्याख्या है,
उसका नाम तटस्थ लक्षण है। इसको अवान्तर वाक्य कहते हैं।
2. जो लक्षण 'मैं' से चराचर के 'मैं' को अभिन्न करके बतावे उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। इसको
महावाक्य कहते हैं।
बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ बिधि नाना ।।
आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी ।।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहइ घान बिनु बास असेषा ।।
असि सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ।।
उपकरण (इन्द्रियों) के द्वारा जो कार्य किया जाय वह लौकिक और बिना उपकरण के जो कार्य किया जाय वह अलौकिक करनी है।
अभी यहाँ बैठे-बैठे सैकड़ों मील दूर किसी देखे हुए स्थान में मन स्मरण करते ही तुरन्त चला गया। दिल्ली, कश्मीर आदि के स्मरण करते ही वहाँ के दृश्य सब दिखने लगे। तब यह मन किस पैर से वहाँ गया? यही 'बिनु पद चलै' है।
आँख से यह दिख रहा है और यह नहीं दिख रहा है, तो 'दिख रहा है' और 'नहीं दिख रहा है' इन दोनों को किस आँख से देखा? यही 'नयन बिनु देखा' है 'कान से सुनाई पड़ रहा है' और 'अब सुनाई नहीं पड़ता' तब कान के सुनने और न सुनने इन दोनों को किसने सुना? यही 'सुनै बिनु काना' है।
सिर के दर्द को किससे छूकर, स्पर्श करके कह रहा हूँ कि अहा! बड़ा दर्द हो रहा है। यही 'तनु बिनु परस' है आदि। ये सब बिना इन्द्रियों के कर्म हो रहे हैं। यही अलौकिक करनी है। यह अलौकिक करनी जिसके द्वारा हो रही है वह 'मैं' आत्मा भगवान है। भगवान आत्मा 'मैं' के ये तटस्थ लक्षण हैं।
आदि अन्त कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ।
राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहिं तहँ मोहनिसा लवलेसा ।।
ये स्वरूप लक्षण हैं।
स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, अज्ञान, अमुक का ही होता है, 'मैं' का नहीं। इसलिए' ही भगवान आत्मा हूँ और इसी को स्वरूप लक्षण कहते हैं।
'राम' शब्द की व्याख्या -
'र', 'अ' और 'म' मिलकर हुआ राम। 'र' है चित्, 'अ' है सत् और 'म'। आनन्द, इस तरह राम का अर्थ हुआ 'सच्चिदानन्द'। जो सत्य होता है, व त्रिकालाबाध्य होता है। जो त्रिकालाबाध्य होता है, वह व्यापक होता है। जो व्यापक होता है, वह निराकार होता है। जो निराकार होता है वह निरंश होता है, जो निरं होता है वह अजन्मा होता है। जो अजन्मा होता है वह अमर होता है। जो अमर होत है, वह एक होता है। जो एक होता है, वह अविनाशी होता है। जो अविनाशी होताहै। वह पूर्ण होता है। जो पूर्ण होता है, वह चित् होता है। जो चित् होता है, वह आनन्दस्वरूप होता है। जो सत्, चित्, आनन्द होता है, वह स्वतः प्रमाण होता है परतः प्रमाण नहीं। जो स्वतः प्रमाण होता है, वह स्वयंवेद्य होता है, परसंवेद्य नहीं जो स्वयंवेद्य होता है वह अहंगम्य होता है, इदंगम्य नहीं। इस तरह 'मैं' आल सच्चिदानंद हूँ।
राम सच्चिदानंद दिनेसा ॥
जिसमें योगी महात्माजन रमते हैं, रमण करते हैं, उन्मत्त रहते हैं, वह है राम प्रश्न है-किसमें योगी महात्मा जन रमते हैं? उत्तर है-जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्न सर्व में व्यापक है, जो सर्व का आधार है, आत्मा है उसमें। इसलिए 'मैं' आत्मा है हुआ राम, ये स्वरूप लक्षण है।
मन की एकाग्रता में जो आनन्द आता है, वह है विषयानन्द और मन की स्थिरत का जो आनन्द है, वह है नित्यानन्द। मन साधना से एकाग्र होता है और यात्रा के परिसमाप्ति में स्थिर होता है। मन एक नदी है, संकल्प विकल्प किनारे हैं, कल्पना धार है। साधन रूपी बाँध से इसे बाँध दो तो वह एकाग्र हो गया। आत्मा रूप सागर पहुँचने पर ही यह मन रूपी नदी स्थिर होती है।
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा ।।
मन का घर तो आनन्द सागर है। वह बिना वहाँ गये स्थिर नहीं हो सकता, वह उसे सुपास होगा।
'आराम' हे राम! आ।
व्यवहारिक जगत में ही देखो, मनुष्य जब सोने लगता है, तब कुछ हल्ला, शोर होता है, तब वह कहता है। अरे! चुप रहो, हमें आराम करना है, अर्थात् शान्ति लेना है। 'आराम' हे राम, आ। तो भैय्या ! शान्ति तो तभी मिलेगी कि जब हृदय में राम आ जायेंगे।
चित्त की चंचलता जाग्रत अवस्था है और चित्त की लय अवस्था सुषुप्ति अवस्था है। सोने की तैयारी में हम बिस्तर पर पड़े हैं, नींद अभी आयी नहीं, आने को है और जाग्रत का अन्त हो रहा है अर्थात् नींद के पूर्व एक ऐसी अवस्था होती है कि उस समय न तो जाग ही रहे हैं और न नींद में ही हैं। यह जाग्रत का अन्त और सुषुप्ति की आदि की अवस्था है। इस समय एक ऐसे विलक्षण आनन्द का अनुभव होते रहता है कि वह 'वृत्ति शून्य' अवस्था ही 'स्वरूप स्थिति' है। इस समय यदि कोई पुकारता है तो वह इस अवस्था का मनुष्य कहता है अरे! अभी चले जाओ कल आना और जो कुछ कहना हो, कहना। अभी हम आराम कर रहे हैं। इतना सब वह कह तो डालता है, परन्तु वृत्ति रहित अवस्था में कहता है। यह अवस्था प्रत्येक में रोज आती है।
सहज प्रकास रूप भगवाना, नहिं तहँ पुनि विज्ञान बिहाना ।।
सहज प्रकाश-जो अंधकार और प्रकाश दोनों का प्रकाशक है, उसे सहज प्रकाश कहते हैं। रात्रि के घोर अंधकार को देखकर हम कहते हैं कि अरे, बड़ा अंधेरा है, टार्च लाओ! इस रात्रि के घोर अंधकार को किस प्रकाश से देखा? रात्रि में तुम स्वप्न देखते हो, स्वप्न में सारा प्रपंच जाग्रत अवस्था के समान ही दिखाई देता है, तब स्वप्न अवस्था में न तो वहाँ सूर्य का प्रकाश है, न चन्द्रमा या बिजली का प्रकाश है और न कोई अन्य प्रकार का ही प्रकाश है, यह सब किसके प्रकाश में देखा जा रहा है, इस स्वप्न के सब व्यवहारों को देखने के लिए, तुम्हारे पास कौन-सा प्रकाश है? यह सब मुझ आत्मा 'मैं' का ही प्रकाश है, जिससे अंधकार और प्रकाश दोनों देखे जाते हैं। यह है सहज प्रकाश। यह बनावटी प्रकाश नहीं है, अकृत्रिम प्रकाश है, परम प्रकाश है।
इस प्रकाश में न रात है, न दिन है। न सुबह है, न शाम है, इसलिए 'सहज प्रकाश रूप भगवाना' 'मैं' आत्मा है। जिससे तीनों काल और तीनों अवस्था नित्य प्रकाशित हैं। सूर्य, चन्द्रमा, बिजली आदि का अन्य प्रकाश, रात के घोर अंधकार को नहीं दिखा सकते। ये प्रकाश अन्धकार के बाधक हैं, परन्तु सहज प्रकाश किसी का बाधक नहीं है।
सहज प्रकाश का अर्थ ज्ञान है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं -
न तद् भासयते सूर्यो, न शशांको न पावकः ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम् ।।
(गीता 15/6, अ-15, श्लो.-6)
जिस प्रकाश को न सूर्य प्रकाशित कर सकता, न चन्द्रमा प्रकाशित कर सकता, अग्नि, न बिजली इत्यादि का प्रकाश प्रकाशित कर सकता वह 'मैं' आत्मा हूँ, परम प्रकाश स्वरूप। इसका अर्थ है कि सूर्य माने नेत्र, आँख का देवता सूर्य है, तब मुझ आत्मा भगवान को आँख नहीं देख सकती, जो आँख को देखता है, वह 'मैं' आत्म हूँ। मन का देवता चंद्रमा है। अतः, मन मुझ आत्मा को नहीं जान सकता। मन को 'मैं' जानता हूँ। ये सब मुझे प्रकाशित नहीं कर सकते 'मैं' इन सबका प्रकाशक है। मानसकार के शब्दों में, यही परमप्रकाश, सहज प्रकाश है।
सहज प्रकास रूप भगवाना। नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना ।।
सहज प्रकाश रूप-अर्थात् सहज ज्ञान ही जिस भगवान आत्मा 'मैं' का स्वरूप है। जहाँ पर विज्ञान रूपी सबेरा नहीं है। किसी भी देश, काल, वस्तु को जानने के लिए 'मैं' आत्मा का ज्ञान, सहज है, स्वाभाविक है, अकृत्रिम है, क्योंकि इनको जानने के लिए 'मैं' आत्मा को किसी की भी अपेक्षा नहीं है। मन को और मन वे सम्पूर्ण व्यवहारों, चित्त को और चित्त के चिन्तन को, बुद्धि को और बुद्धि के निश्चया और अनिश्चय को 'मैं' आत्मा बिना किसी अन्य की सहायता के स्वयं ही जानता हूँ जाग्रत, स्वप्न के सब प्रपंच को और सुषुप्ति के आनन्द का अनुभव 'मैं' स्वयं करत हूँ। तीनों काल को जानता हूँ। 'मैं' आत्मा कितना ज्ञान स्वरूप, ज्ञान पुञ्ज, ज्ञान भण्डार हूँ कि मुझमें जाननापना में कभी कमी नहीं होती। 'मैं' अखण्ड ज्ञान स्वरूप हूँ। जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक जानता रहूँगा और सृष्टि के अन्त के बाद भी जानने का अन्त नहीं होगा। इसलिए 'मैं' आत्मा ज्ञान पुञ्ज अखण्ड ज्ञान स्वरूप, सहर प्रकाश हूँ। जिसका जानना सहज है। यदि स्वयं सहज न हो तो जानना भी सहज हो, तब जो स्वयं सहज है तो उसका जानना भी स्वयं सहज है।
'मैं' हूँ यह कहना, सबके लिए सहज है, इसका जानना अनुभव करना, कहना सबके लिये सर्वदा सहज है। किसी को इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होती। 'मैं आत्मा सहज हूँ, तो सब सहज है। देखना, सुनना, ज्ञान, अनुभव आदि सब मुः आत्मा का सहज है, यहाँ पर सब साधनों की परिसमाप्ति हो जाती है। भगवान के कठिन मानकर ही तो साधन किये जाते हैं।
सहज ही सहज को अनुभव करता है। सारे चराचर का ज्ञान, इस तरह नित्य सहज है। जानना ही मुझ आत्मा की आँख है, जानना ही मुझ आत्मा का कान है, जानना ही मुझ आत्मा का घ्राण है, जानना ही मुझ आत्मा की त्वचा है, जब 'मैं' स्वयं के लिए सहज हूँ, तब औरों के लिए भी सहज हूँ। जो मुझ आत्मा को कुछ करके जानना चाहता है, उसके लिए कठिन हूँ और जो बिना कुछ किये जानना चाहता है, उसके लिए 'मैं' आत्मा नित्य सहज हूँ।
परमानंद, परेस पुराना ।।
आनन्द और निरानन्द दोनों को जो जानता है, उसे परमानन्द कहते हैं। 'परेश' का अर्थ है 'परा' अर्थात् माया, 'ईश' अर्थात् स्वामी, पति, आधारा इस तरह परेश का अर्थ है, माया का स्वामी, माया का आधार, रक्षक।
'पुराना' अर्थात् जुन्ना, अनादि, सनातन, बिना जन्म कुण्डली का, अजन्मा, अविनाशी।
ज्ञान और अज्ञान दोनों से 'मैं' परे हूँ ऐसा जो जानता है, वह 'मैं' आत्मा हूँ और ऐसा जो नहीं जानता, वह है 'जीव'।
कोई कहता है भगवन्! मैं तो अज्ञानी हूँ और आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। ऐसा कहने वाला, जो ज्ञान को भी जान रहा है और अज्ञान को भी जान रहा है और दोनों को जानकर, एक को ज्ञानी और अपने को अज्ञानी कह रहा है, वह कहने वाला कौन है? ज्ञान को जानकर उसे मुझ पर आरोपित किया और मुझे ज्ञानी कहा और अज्ञान को जानकर उसे अपने पर आरोपित करके अपने को अज्ञानी कहा। तो आरोपित की जाने वाली चीज अलग और जिस पर आरोपित किया जा रहा है वह इनसे अलग। जैसे-टोपीवाला कहा जाता है, तब टोपी अलग और जिस पर टोपी आरोपित है, वह अलग। इसी तरह ज्ञान और अज्ञान ये अलग और जिन पर इनको आरोपित किया, वह इनसे अलग, तो वह जो इन दोनों से अलग है वही कह रहा है तब वह कौन है? वही स्वयं है, 'मैं' आत्मा, राम। तब, जब वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तब अज्ञानी कहाँ रहा।
जो ज्ञान, अज्ञान का नाश करता है, वह है विशेष ज्ञान और जो ज्ञान, अज्ञान को जानता है, वह है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान व्यापक है, यह सब में व्याप्त है। बाँस में सामान्य अग्नि व्यापक है, दो बाँस को रगडो, तो उसमें की वही सामान्य अग्नि विशेष रूप ग्रहण करके बॉस को जलाकर फिर सामान्य का सामान्य हो जाती है।
इसी तरह गुरु-शिष्य के विचार रूपी रगड़ से विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। सामान्य ज्ञान, सहज ज्ञान है, यही सहज स्वरूप है, यही आत्मा है, यही राम है।
हरष, विषाद, ग्यान, अग्यान, जीवधरम, अहमिति अभिमाना ।।
हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान आदि मान्यता जगत् में है, ये सब जीव देश में ही हैं, आत्म जगत् में नहीं। सम्पूर्ण विकार जीव धर्म में ही है, जीव की मान्यता में ही सम्पूर्ण विकार है, आत्म जगत् में नहीं। आत्मा जान लेने पर सम्पूर्ण विकारों का अभाव हो जाता है।
प्रश्न- इसका क्या प्रमाण है?
उत्तर- अपने आपको आत्मा जानकर देख लो। यही इसका प्रमाण है।
प्रश्न- अपने आपको आत्मा जानना क्या है?
उत्तर- अपने आप को कुछ भी नहीं मानना, यही, अपने आपको आत्मा जानना है।
"राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानन्द परेश पुराना" का यही भाव है।
दोहा-
पुरुष, प्रसिद्ध, प्रकास निधि, प्रगट, परावर नाथ ।
रघुकुल मनि, मम, स्वामि सोइ, कहि सिर्वं नायउ माथ ।।
(बा.कां.-116)
जो पुरुष है, यह शब्द लिंग वाचक नहीं है, 'पु' माने पुरी (शरीर) इसके भीतर जो विश्राम करता है (आत्मा) उसे पुरुष कहते हैं। वही सच्चिदानन्द घनभूत आत्मा है।
प्रकृतिविकृतिभिन्नः शुद्धबोधस्वभावः
सदसदिदमशेषं भासयन्निर्विशेषः ।
विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववस्था-
स्वहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः ।।
(137-विवेक चूड़ामणि)
प्रकृति माने कारण और विकृति माने कार्य। न तो भगवान किसी से पैदा हुआ और न भगवान से कोई पैदा हुआ। प्रकृति, विकृति अर्थात् कारण-कार्य से रहित, शुद्ध बोध ही जिसका स्वभाव है।
जिस परमात्मा से जगत् की उत्पत्ति मानते हो, वह परमात्मा, जन्मा है या अजन्मा ?
जन्मा मानने पर उसे विनाशी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो जन्म लेगा वह मरेगा और यदि वह जन्मा है तो वह किससे जन्मा ? फिर, जिससे वह जन्मा, उसको किसने जन्म दिया, फिर उसका जन्मदाता कौन? और अजन्मा मानने पर, जब वह स्वयं पैदा नहीं हुआ तब उसे दूसरे को जन्म देने की क्या तमीज, जो दूसरे को जन्म देगा। न्याय से वेदान्त का प्रश्न है-तुम्हारा ईश्वर, जिसने तुम्हारे सिद्धान्त के अनुसार, जगत् की रचना की, वह साकार है या निराकार? यदि साकार है तो वह नित्य नहीं हो सकता और यदि निराकार है तो व्यापक होने के नाते, अक्रिय और अकर्त्ता है। इस तरह दोनों से जगत् की रचना, ईश्वर के द्वारा सिद्ध नहीं होती।
भगवान, शुद्ध बोध स्वरूप है, यही स्वभाव है। अशुद्ध बोध मान्यता ही है शुद्ध बोध 'मैं' का 'मैं' ही जानना है। तीनों काल और तीनों अवस्थाओं का जानना (भोगना) यही इसका विलास करना है, इस पुरी (शरीर) के अन्दर उसे हम कैसे जानें? इसका उत्तर है-अरे, जो सोऽहं, सोऽहं, सोऽहं करके नित्य कहते जा रहा है, वह 'मैं' हूँ, 'मैं' हूँ, ऐसा अहर्निश बोल रहा है, ऐसा जानना ही, उसे जानना है, वह कार्य, कारण से भिन्न है, सर्व से परे, सर्व का दृष्टा है, सर्व उसे नहीं जान सकते, जो सर्व को जानता है, वह आत्मा 'मैं' राम है। जिसके बिना जिसका अस्तित्व एक क्षण के लिए भी न रह सके, वह उसकी आत्मा है। जो जिसका कारण होता है, वह उसका आधार होता है, वह उसमें व्यापक होता है, वह उसका सर्व होता है, ऐसा भगवान सबमें 'मैं' हूँ, 'मैं' हूँ, इस तरह नित्य व्यक्त हो रहा है। प्रसिद्ध है।
शुद्ध बोध क्या है और अशुद्ध बोध क्या है? अपने आप 'मैं' आत्मा को कुछ भी मत माने, 'मैं' का 'मैं' ही जाने, इसको शुद्ध बोध कहते हैं और अपने 'मैं' आत्मा को कुछ भी माने इसको अशुद्ध बोध कहते हैं।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा, समाधि इन सबका अनुभव 'मैं' आत्मा सतत् करते रहता हूँ। अगर, इनको न जानूँ तो इनका अनुभव कौन बताएगा? इसलिए जानना ही जिसका स्वभाव है। यही शुद्धबोध है।
अनादिकाल से 'मैं' आत्मा जानते आ रहा हूँ, परन्तु आज तक मुझ आत्मा के जाननापने में कमी नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई! अब हम बहुत जान गये, हमारा जाननापना खतम हो गया, जब थोड़ा जाननापना और इकट्ठा हो जाने दो, तब फिर जानेंगे। रात-दिन मुझ आत्मा का जानना ही स्वभाव है, इसलिए 'मैं' आत्म ज्ञान स्वरूप, ज्ञान पुञ्ज, ज्ञान का भण्डार ज्ञानघन अर्थात ठोस। 'मैं' आत्मा ठोस ज्ञान स्वरूप हूँ।
किसी भी देश-काल, वस्तु को जानने के लिए मुझे समयऔर सीमा की अपेक्षा नहीं कि 'मैं' कितनी जल्दी जानता हूँ। कोई भी वस्तु ज्यों ही सामने आयी कि उसे तत्काल जानता हूँ, 'प्रज्ञानम् ब्रह्म', अर्थात् जो तत्काल ही जाने। इसलिए, 'मैं' ज्ञान स्वरूप हूँ। कितना ज्ञान है, इसकी कोई थाह नहीं, अथाह है। इसलिए 'मैं' आत्मा-ज्ञान निधि हूँ। ज्ञान का समुद्र हूँ। बुद्धि रूपी बर्तन में जितना भर लो इस ज्ञान समुद्र में कमी कभी नहीं होना है। वह तो ज्यों का त्यों है। जितना का उतना है, जैसा का तैसा है, जरूरत तो अपनी बुद्धि रूपी पात्र को बडे बनाने का है। फिर, तो जितना चाहो, उतना भर लो, इस ज्ञान के भण्डार में कमी कभी होने की नहीं है।
मुझ आत्मा का जाननापना, नित्य तीनों काल और तीनों अवस्था में, अनादिकाल से एक रस है, यह कभी खण्डित नहीं होता। इसलिए 'मैं' आत्मा अखण्ड ज्ञान स्वरूप हूँ।
'मैं' क्या नहीं जानता, किसको नहीं जानता, इन्द्रियों से गुप्त होने के कारण 'मैं' गुह्य और स्वयं के द्वारा नहीं जानने के कारण 'मैं' परमगुह्यज्ञानस्वरूप हूँ। वाणी कथन करती है, इसको भी 'मैं' जानता हूँ और चुप हो जाती है, इसको भी 'मैं' जानता हूँ, परन्तु चुप होना और बोलना ये मुझे नहीं जान सकते, इन दोनों की सिद्धि 'मैं' ही करता हूँ। अब कौन है, जिसके सामने 'मैं' व्यक्त होऊँ? या व्यक्त करूँ? यह स्वयं करके नहीं जानता है? यही आलस्यधुरीण पद है, इस अनुभूति में जो निर्विकल्पता और निस्तब्धता आ गयी, इन दोनों को 'मैं' जान रहा हूँ। ये दोनों भी 'मैं' नहीं हूँ, इन दोनों की सिद्धि भी मुझ करके ही है, वह 'मैं' आत्म ज्ञान स्वरूप, इन दोनों से परे हूँ।
'मैं' भिन्न होकर जानता हूँ या अभिन्न होकर जानता हूँ या भिन्नाभिन्न होकर जानता हूँ या वही होकर जानता हूँ?
उत्तर है-वही होकर जानता हूँ।
यदि, इस तरह जानता हूँ तो फिर ये है ही नहीं, तब जानता किसको हूँ? किसी को नहीं।
बस, इस अनुभूति की जो अनुभूति हो रही है, वही 'मैं' आत्मा ज्ञान स्वरूप की स्वरूपस्थिति है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। 'मैं' आत्मा ज्ञान स्वरूप, चैतन्य घनभूत, लबालब परिपूर्ण हूँ। जो मनगम्य, बुद्धिगम्य, चित्तगम्य, वाणीगम्य नहीं हूँ। अहंगम्य और अनुभवगम्य हूँ।
जो बेसहारा, इस गुल चमन का, उस बेसहारे को हम भी जाने ।
जो नूरेहस्ती है बेकिनारा, उस बेकिनारे को हम भी जानें ।
तरह-तरह की बेशुमार कलियाँ, कभी सिकुड़तीं, कभी उघड़तीं ।
जो इश्क ये दिल है, मिश्ले-मजनूं, तलाश करता है कूचे-कूचे।
मिटती है मिलते ही ख्वाहिशातें, माशूक्रे - लैला को हम भी जानें।
जो जानता है जहान सारा, जो देखता है हमेशा सबको ।
पहचान जिसको भले-बुरे की, पहचान वाले को हम भी जानें ।।
रहता है सबमें हो करके सब कुछ, वेइब्तिदा और वेइन्तिहा है ।।
मशरू.फ़ रहते हैं मस्त जिसमें, उस मस्त सूरत को हम भी जानें ।।
अनमोल 'मुक्ता' का ये खजाना, गर लूटना है, मजे से लूटो ।
हक़ीक़ी मस्तों की जो हक़ीक़त, ऐसी हक़ीक़त को हम भी जानें ।।
पुरुष, प्रसिद्ध प्रकास निधि -
जो पुरुष है, 'मैं' आत्मा वह प्रसिद्ध है। तीनों काल और तीनों अवस्थाओं में वह नित्य प्रसिद्ध है। उसका कभी अभाव नहीं होता यही प्रसिद्ध है। वह अव्यक्त और व्यक्त रूप में, नित्य प्रसिद्ध है। अस्तित्व सामान्यचेतन 'है' है, इस रूप में जो नित्य है। संसार में ऐसा कोई है, जो 'है' इस अस्तित्व से खाली हो। ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, जीव है, ब्रह्म है, ज्ञान है, अज्ञान है, भाव है, अभाव है, है है, नहीं है, पाप है, पुण्य है, स्वर्ग है, नरक है आदि जो तृण से लेकर ब्रह्मा तक 'है' रूप से प्रसिद्ध है, यही अस्तित्व, सामान्य चेतन 'है' है, इस रूप में जो नित्य है।
जो वाणी से न कहा जाय, अव्यक्त चेतन 'है' का ही व्यक्त रूप 'मैं' है। 'है' जो 'मैं' नाम से नित्य व्यक्त हो रहा है। प्रसिद्ध हो रहा है। इस तरह वह व्यक्त और अव्यक्त रूप में नित्य प्रसिद्ध हो रहा है। 'है' सामान्य चेतन और 'मैं' विशेष चेतन इन दोनों को आत्म भाव से प्राप्त करना चाहिए।
विषय समझो डण्डा 'है'।
प्रश्न होता है कि डण्डे का यह जो 'है' है, (पहला 'है' कर्त्ता, दूसरा 'है' क्रिया है) यह, डण्डे का 'है' है या लकड़ी का 'है' है?
उत्तर है- लकड़ी का 'है' है। यह जो प्रतीत हो रहा है, भान हो रहा है, वह लकड़ी ही तो है, डण्डा नहीं। क्योंकि, यदि डण्डे से लकड़ी निकाल लोगे तो डण्डा नहीं रह सकता, फिर भान या प्रतीति किसकी होगी। अतः, सिद्ध हुआ कि यह जो डण्डे में 'है' पना है, वह डण्डे का नहीं, लकड़ी का है। आगे चलो-अब लकड़ी 'है' इस लकड़ी में जो 'है' है, वह लकड़ी का है या पृथ्वी का है? उत्तर है-पृथ्वी का। क्योंकि यदि लकड़ी में से पृथ्वी निकाल लोगे, तो लकड़ी रहेगी कहाँ ? इससे, सिद्ध हुआ कि यह जो लकड़ी का 'है' है, वह लकड़ी का नहीं बल्कि पृथ्वी का 'है' है। इस तरह, पृथ्वी का जो 'है' है, वह जल का 'है' है। जल का जो 'है' है, वह अग्नि का 'है' है। अग्नि का जो 'है' है, वह वायु का 'है' है। वायु का जो 'है' है वह आकाश का 'है' है और आकाश का जो 'है' है वह मुझ आत्मा, चैतन्यघनभूत का 'है' है। इस तरह वह अव्यक्त रूप से नित्य व्यक्त हो रहा है। प्रसिद्ध है। इसी तरह व्यक्त रूप 'मैं' नित्य प्रसिद्ध है, जिससे भी पूछो भाई! तुम कौन हो? उत्तर मिलेगा 'मैं' हूँ। सारा विश्व अपने आपको 'मैं' भाव से व्यक्त करता है। इस तरह 'मैं' (विशेष चेतन) इस भाव में, सर्व में, नित्य व्यक्त हो रहा है। अब यदि डण्डे से पूछोगे कि तुम कौन हो तो वह भी यही कहता है, कि 'मैं' हूँ, परन्तु वह एक गुण तमोगुण का ही है, उसमें रजोगुण अर्थात् इन्द्रियाँ और सतोगुण अर्थात् बुद्धि का अभाव है, अतः वह बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, परन्तु अव्यक्त रूप 'है' है। इस अस्तित्व सामान्य चेतन से नित्य प्रसिद्ध है।
चारों प्रमाणों से अपना अस्तित्व सिद्ध है।
1. प्रत्यक्ष प्रमाण, 2. अनुमान प्रमाण, 3. निगम प्रमाण और 4. स्वानुभूति प्रमाण ये ही चार प्रमाण हैं।
मानने से रहे और न मानने से भी रहे, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है।
आज नदी में बाढ़ आ गयी। यद्यपि, यहाँ पानी नहीं गिरा, तब यह निश्चय है कि ऊपर कहीं पानी गिरा होगा। यह अनुमान प्रमाण है।
वेद, शास्त्र, रामायण, गीता, भागवत सभी यही बताते हैं कि भगवान आत्मा 'मैं' के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, यही निगम प्रमाण है।
"मैं" हूँ इसको स्वयं में ही जानता हूँ यही स्वानुभूति प्रमाण है।
सारांश में समझो, 'मैं' हूँ यह प्रमाण सबके लिए प्रत्यक्ष है, यही 'मैं' के लिए दृढ़ प्रत्यक्ष प्रमाण है।
यदि, 'मैं' नहीं होता, तो कहता कौन कि 'मैं' हूँ, यही दृढ़ अनुमान प्रमाण है।
यदि 'मैं' नहीं होता तो भीतर से बोलता कौन कि 'मैं' हूँ, यह दृढ़ निगम प्रमाण है। इन तीनों प्रमाणों को 'मैं' जानता हूँ, यही दृढ़ स्वानुभूति प्रमाण है।
जैसे, प्रकाश को प्रकाश से ही देखा जाता है। अंधकार, प्रकाश को क्या दिखा सकेगा, ऐसे ही 'मैं' को 'मैं' के ही द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है। वेद, शास्त्र, पुराण, श्रुति, स्मृति ये सब अनात्म है। ये सब मुझ आत्मा को क्या दिखा सकेंगे? तब शंका होती है कि जब ये मुझ आत्मा को नहीं दिखा सकते, तब इनकी अन्यथा सिद्धि है, ये सभी व्यर्थ है?
भाई! मुझ सच्चिदानन्द के भाव की व्याख्या नहीं हो सकती, जो तत्त्व, अपने आप से ही जाना जाता है, उसकी व्याख्या अगर शास्त्रों में हो तो फिर हम तुम्हें क्या जनाएँगे? जिसको तुम जानते हो, उसी को हम जनाते हैं। तो स्वामी जी! मैं किसको जानता हूँ।
भैय्या! जो सबको जानता है, उसी को जानते हो। सन्त, महात्मा जन उसी को जनाते हैं। प्रश्न- जब मैं पहिले से ही जानता हूँ, तब आप क्या जनाते हैं? भाई! हम यही जनाते हैं कि तुम पहिले से ही जानते हो। अरे, 'मैं' हूँ, इसको जानते हो या नहीं? जी हाँ जानता हूँ। तो और क्या जानोगे? कोई सींग, पूँछ वाला जानना है? नहीं। इसी को हम जनाते हैं। अपने आप 'मैं' आत्मा को, तुम कुछ न कुछ मान कर जानते हो, उसी को सन्त, महात्मा जन जान कर जनाते हैं।
प्रश्न- तुम मानकर कैसे जानते हो? देखो! तुम कहते हो- 'मैं' देह हूँ, 'मैं' स्त्री हूँ, 'मैं' पुरुष हूँ, 'मैं' बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ, ब्राह्मण हूँ, गृहस्थ हूँ, माता- पिता, भाई-बहिन हूँ आदि। तुमने अपने आप 'मैं' को, देह माना, स्त्री-पुरुष माना, बालक, युवा, वृद्ध माना, वर्ण, आश्रम वाला माना, माता-पिता, भाई-बहिन माना।
इस तरह तुम कुछ न कुछ मानकर जानते हो। 'मैं' को जानते हो, अपने 'मैं' का ज्ञान है और देह जो मान रहे हो, इस देह का भी ज्ञान है। अब विचार करो कि यह जो तुमने देह माना, वह किसको माना? उत्तर है 'मैं' आत्मा अस्तित्व को, 'है' को। तब देह, देह है या अस्तित्व, 'मैं' आत्मा?
उत्तर- अस्तित्व है, ' मैं' आत्मा है।
तब देह रहा? नहीं।
तब क्या रहा?
उत्तर है- 'मैं' ही रहा।
इस तरह सब मान्यताओं का अभाव है। 'मैं' ही 'मैं' हूँ। बस, हम यही जनाने आये हैं। जिसको देह कहते हो, प्रपंच कहते हो, वह 'मैं' ही है। यह देह है, इसको अध्यास कहते हैं और देह मानकर, 'मैं' देह हूँ कहना अभिमान है। मान्यता अध्यास है और वह 'मैं' हूँ कहना अभिमान है। 'है' और 'मैं' अव्यक्त और व्यक्त दोनों भाव से 'मैं' आत्मा, नित्य प्रसिद्ध है।
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निघि
जो पुरुष है, वह प्रसिद्ध है, फिर वह प्रकाश निधि है।
प्रकाश निधि का अर्थ होता है, प्रकाश पुञ्ज, जो न कभी उदय हो और न कभी अस्त हो। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान और अंधकार का अर्थ होता है अज्ञान। जिससे प्रकाश और अंधकार दोनों देखे जाते हैं, वह है प्रकाशनिधि। वह प्रकाश न कभी उदय होता है और न अस्त। यह सर्व का ज्ञाता है।
प्रकाश निधि - प्रकाश माने ज्ञान, निधि माने समुद्र अर्थात् ज्ञान का समुद्र।
ग्यान अखण्ड एक सीताबर, माया वस्य जीव सचराचर ।।
वह ज्ञान अखण्ड है, कभी खण्डित होने वाला नहीं है। खण्ड ज्ञान क्या है? किसी उपकरण (इन्द्रिय) के द्वारा जो जाना जाय, वह खण्ड ज्ञान है और बिना उपकरण के जो जाना जाय वह अखण्ड ज्ञान है। भगवान आत्मा 'मैं' अखण्ड ज्ञान स्वरूप है। देखो! (ताली बजाकर) यह ध्वनि हुई। इसे किसने सुना? कर्ण इन्द्रिय ने और कर्ण इन्द्रिय के सुनने को किसने सुना? 'मैं' आत्मा ने। तो, जो सुनने और नह सुनने दोनों को सुनता है, देखने और नहीं देखने, दोनों को देखता है (बिना उपकरण के) वह 'मैं' आत्मा अखण्ड ज्ञान स्वरूप हूँ। जो सुषुप्ति के आनंद का अनुभव बिन उपकरण के करता है, वह 'मैं' आत्मा ज्ञानस्वरूप अखण्ड हूँ। इन्द्रियों का ज्ञान खण्ड ज्ञान है और "मैं" आत्मा का ज्ञान अखण्ड ज्ञान स्वरूप है। वह अखण्ड ज्ञा अनेक नहीं एक है। तीनों अवस्था और तीनों काल का ज्ञान जो है, वह नित्य एक रह अखण्ड है। इस अखण्ड ज्ञान में देशकाल का अत्यन्ताभाव है। इसलिए 'ग्यान अखण् एक सीताबर' है। यही प्रकाश का समुद्र है, जो आदि अन्त से रहित है।
पदार्थ दो प्रकार के होते हैं 1. दृष्ट पदार्थ, 2. अदृष्ट पदार्थ। जो देखने में आवे, उसे दृष्ट पदार्थ और जो देखने-सुनने में न आये, उसे अदृष्ट पदार्थ कहते हैं।
जगत्, प्रपंच, संसार, विश्व, अश्वत्थ ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब अदृष्ट हैं। आकाश, वायु (ये सब) अग्नि, जल, पृथ्वी ये पाँचों प्रपंच हैं। ये सब मिलकर एक जगह रहें, तब उसे प्रपंच कहते हैं।
संसार-संसरणम् संसारः। पता चलाने चलो, पकड़ने चलो तो जो सरकता चला जाय, अपनी जगह पर न मिले, इसको ढूँढने चलते हैं, तो यह आगे-आगे सरकता चला जाता है, मिलता नहीं, इसलिए इसका नाम संसार है।
जगत्-गच्छन्तियः सः जगत्-जिसको निश्चय करने चलो, तो वह आगे-आगे सरकता चला जाता है, उसे जगत् कहते हैं।
विश्व-वि, माने विगत, श्व माने प्रातः। रात के अंधेरे में तो रहे और प्रातः प्रकाश में जो विगत हो जाय अर्थात् न रहे। अज्ञानके अंधेरे में तो रहे, पर ज्ञान के प्रकाश में न रहे, उसे कहते हैं विश्व।
अश्वत्थ- 'अ' माने नहीं, 'श्व' माने प्रातः, 'थ' माने स्थिर। जो रात के अंधेरे में तो रहे और प्रातःकाल के प्रकाश में जो स्थिर न रहे, उसे अश्वत्थ कहते हैं। मान्यता अश्वत्थ है, वृक्ष है, इसमें जो सत्यता प्रतीत होती है, वह अज्ञान के अंधेरे में ही होती है। अनन्त मान्यताओं का जो समूह है, उसे संसार कहते हैं। अनन्त- मान्यताओं का जो आधार है वह अस्तित्व ही है। यह संसार सब प्रकार से पूर्ण है।
प्रश्न होता है-क्यों ?
उत्तर है- अरे, इसका बाप भी तो पूर्ण है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई। पूर्ण पिता से पूर्ण पुत्र की उत्पत्ति होती है। बाप के दो आँख, दो कान, दो हाथ, दो पैर हैं, तो बेटा एक आँख, एक कान, एक हाथ और एक पैर वाला, ऐसा अपूर्ण नहीं होता। बाप के सब दो-दो, तब बेटे के भी सब दो-दो। बाप-बेटे दोनों पूर्ण हैं। इसी तरह 'मैं' आत्मा अस्तित्व, अनादि है, अविनाशी है, अनिर्वचनीय है, तब संसार भी वैसा ही है। अब प्रश्न होता है कि संसार के उपरोक्त विशेषण संसार के हैं या भगवान आत्मा के? उत्तर है, भगवान आत्मा के हैं। यही भगवान (बाप) का गुण, संसार (बेटे) में है। अतः, जिसे भगवान कहते हो, जो राम है, 'मैं' आत्मा, वही दृष्ट पदार्थ है, शेष सब प्रपंच, अदृष्ट हैं। उन्हें देखने, अनुभव करने चलो तो वे नहीं मिलते। मान्यता प्रपंच देश है, इसका आधार भगवान देश है। प्रपंच देश में प्रपंच है और भगवान देश में सब भगवान ही है।
भगवान देश में खड़े होकर देखो, ब्रह्मा से लेकर तृण तक, कण-कण, जरी, वर्रा भगवान है। उससे एक तिल भर भी जगह खाली नहीं है।
सर्व में से अमुक भाव हटा दो, विकल्प त्याग दो, फिर तो वही-वही है। वह दू नहीं है। इसका आनन्द तो तभी आयेगा, जब तुम अमली जामा पहिनोगे। इसक बिना, वह आनन्द दूर है। मानसकार विनय में कहते हैं-
हे हरि ! कवन जतन सुख मानहु ।
ज्यों गज-दसन तथा मम करनी, सब प्रकार तुम जानहु ।
जो कछु कहिय-करिय, भव सागर तरिय बच्छपद जैसे ।
रहनि आन विधि, कहिय आन हरिपद सुख पाइय कैसे ।।
देखत चारु मयूर बयन सुभ बोलि सुधा इव सानी ।
सविष उरग आहार, निठुर अस यह करनी वह बानी ।।
अखिल-जीव-वत्सल, निरमत्सर चरन-कमल-अनुरागी ।
ते तव प्रिय रघुबीर धीरमति, अतिसय निज पर त्यागी ।।
हे हरि मैं किस प्रकार सुख मानूँ। मेरी करनी हाथी के दिखावटी दाँतों के समा है। भाव यह है कि जैसे हाथी के दाँत दिखाने के और तथा खाने के और होते हैं, उसे प्रकार मैं भी कहता (दिखाता) कुछ और हूँ और करता कुछ और ही हूँ। मैं दूसरों जो कुछ कहता हूँ, वैसा ही यदि स्वयं करने भी लगूँ तो भवसागर से बछड़े के खुर निशान में भरे हुए जल को सरलतापूर्वक लांघ जाने की भाँति अनायास ही ता जाऊँ, परन्तु करूँ क्या, मेरा आचरण तो कुछ और है और कहता कुछ और हूँ, फि भला तुम्हारे चरणों का यह परमपद का आनन्द कैसे मिले ?
मोर देखने में तो सुन्दर लगता है और अमृत से सने हुए मीठी बोली बोलता है परन्तु उसका भोजन जहरीला साँप है। वह साँप खाता है। कैसा निष्ठुर है? करनी वह (जहरीले सर्प खाना) और कथनी (अमृत से सने हुए मीठी बोली बोलना मानसकार कहते हैं, हे नाथ! तुमको तो वे सन्त प्यारे हैं, जो धीर, गंभीर और राग द्वेष से रहित हैं। जिनने, अपने-पराए का भेद बिल्कुल त्याग दिया है। अर्थात् सब एक तुमको ही देखते हैं।
जद्यपि मम् अवगुन अपार, संसार-जोग्य रघुराया ।
तुलसिदास निज गुन बिचारि, करुनानिधान करु दाया ।।
(विनय पत्रिका पद-118
इस वट वृक्ष के बीज को देखो। वह कितना सूक्ष्म है। इसमें यह इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। वह बीज, स्वयं वृक्ष रूप होकर इसके पत्ते, डालियाँ जड़, पींड, फूल-फल सबमें समाया हुआ है। इसी प्रकार भगवान आत्मा स्वयं जगत् प्रपंच का बीज है। यह प्रपंच उसी से पैदा हुआ है। इस प्रपंच की उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा हुई तथा वह स्वयं बीज की भाँति इसमें समाया हुआ है। अरे, अधिक क्या कहें, बीज ही तो है, जो स्वयं वृक्ष है। इस तरह ज्ञान और अज्ञान दोनों को प्रकाशित करने वाला 'मैं' आत्मा प्रकाशनिधि है।
'प्रगट परावरनाथ'
वह पुरुष, प्रसिद्ध प्रकाशनिधि होते हुए प्रगट है। सब अपने को 'मैं' नाम से नित्य व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए वह नित्य है (इस व्यक्त रूप में) और सारा चराचर, मान्यता रहित प्रतीयमान भास, भगवान के भाव में 'है' है, अस्तित्व रूप में नित्य प्रकट है, प्रत्यक्ष है।
प्रश्न- आकाश विकल्प है या वस्तु है?
विकल्प कहो तब आकाश नहीं, क्योंकि विकल्प अस्तित्वहीन होता है और आकाश यदि वस्तु है तो भी आकाश नहीं, तब फिर यह क्या है? तब यह जो है, सोई है। जैसा है, वैसा ही है। जहाँ है, वहीं है। बस, इस रूप में वह नित्य प्रगट है।
बिस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन बिस्वासु ।
लोक कल्पना बेद कर, अंग अंग प्रति जासु ॥
शरीर का विकल्प हुआ। अब जिस पर शरीर का विकल्प हुआ, वह इस शरीर विकल्प से ढँक गया। अब इस विकल्प को हटा दो, तब क्या रह गया? इस पर कुछ भी विकल्प मत करो, अब यह जो प्रतीयमान (भास) शेष रह गया है, जो मन, वाणी का विषय न रहा, जो अनुभवगम्य है, वही 'मैं' आत्मा हूँ, जिस पर सारा विश्व आधारित है।
प्रश्न-विकल्प हटाने का साधन क्या है?
उत्तर- विकल्पक के बोध में, विकल्प का अभाव है।
प्रश्न-विकल्पक का बोध, कैसा होता है?
उत्तर-विकल्प, विकल्प है या विकल्प वस्तु है? यदि विकल्प, विकल्प है। विकल्प, विकल्प नहीं, वस्तु ही है 'मैं' आत्मा है और यदि विकल्प वस्तु है, तथा विकल्प, विकल्प नहीं वस्तु है, 'मैं' ही हूँ। यही विकल्प हटाने का साधन है ॐ यही विकल्पक का बोध है। इसलिए -
बिस्व रूप रघुबंस मनि, करहु बचन बिस्वासु ॥
इस रूप में नित्य प्रगट है।
'शरीर है'। यहाँ अब, प्रश्न उठता है कि शरीर, शरीर है या 'है' शरीर है?
उत्तर- 'है' शरीर है, 'है' (अस्तित्व) शरीर है।
प्रश्न- मन, मन है या 'है' मन है? 'है' विषय है।
उत्तर - 'है' (अस्तित्व) मन है।
विषय, विषय है या 'है' विषय?
विश्व, विश्व है या 'है' विश्व है? 'है' विश्व है। बस-
बिस्व रूप रघुबंस मनि, करहु बचन बिस्वासु ॥
इस रूप में नित्य प्रगट है। जब देह नहीं रहा तब देहाभिमान नहीं रहा। ज देहाभिान नहीं रहा, तब जीने मरने का डर नहीं रहा। इस स्थिति में देश, काल वस्तु का अत्यन्ताभाव हो गया। सिवा चैतन्यघन भूत, 'मैं' आत्मा के कुछ भी शे नहीं रहा, यही निर्भय पद है, आत्म पद है-परम पद है।
संसार के प्रत्येक पदार्थ में पाँच अंश होते हैं। अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। इसमें प्रथम तीन अंश-अस्ति, भाति और प्रिय भगवान राम, 'मैं' आत्मा हैं।
विषय समझो - विकल्प हटा देने के बाद जो रह गया, उसे वाणी व्यक्त नहीं क सकती, उस पर सोचना, विचारना, बन्द हो गया, परन्तु उसकी प्रतीति तो हो र है, भान तो हो रहा है कि कुछ है, यही अस्तित्व है, 'है' है। इसी को अस्ति कहते है जो सत् है। यह अस्तित्व जो भास रहा है, वही भाति है अर्थात् भासता है, वह वि (चेतन) है और जो अस्ति, भाति है अर्थात सत् चित् है, वही प्रिय है, आन स्वरूप है। इस तरह सारा चराचर सत्, चित्, आनन्द (सच्चिदानन्द) के रूप में नित्य प्रगट है।
बिस्व रूप रघुबंस मनि, करहु बचन बिस्वासु ।।
अस्ति, भाति, प्रिय ये तीन अंश, भगवान राम हैं, अब इस पर, नाम और रूप का विकल्प कर लिया गया, इस तरह दो अंश, इसमें और जुड़ गये। जिसमें 'मैं' आत्मा भगवान छिप गया, यही दो अंश माया के हैं, यह जो मान्यता है, विकल्प है, यही माया है, सीता है। अतः, सारा चराचर सीय राममय हुआ। श्री मानसकार कहते हैं-
सीय राम मय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ।।
का यही भाव है। इस रूप में वह नित्य प्रगट है- 'गुप्त प्रगट वह है नहीं, सरासरी मैदान' ।
गुप्त प्रगट वह है नहीं, सरासरी मैदान ।
ब्रह्मदत्त द्विज देख लो, बिन आँखी बिन कान ।
भाई ! आँख, कान का यहाँ क्या काम, यह इन्द्रियगम्य नहीं है, अहंगम्य है।
नियरे है दीखै नहीं, घिक है ऐसे जिन्द ।
तुलसी या संसार को, भयो मोतिया बिन्द ।।
है सो नजर न आवही, नहीं सो प्रगट दिखाय ।
यह कौतुक तब ही लखै, जब सद्गुरु मिल जाय ।।
बेखुदी का दरिया उमड़ रहा, कब क्या हो जाये ख़ुदा जाने ।
जब डूब गया आलम सारा, कब क्या हो जाये ख़ुदा जाने ।।
झर रही है मस्त बादलों से, मुतवातिर मदमाती बूंदे ।
दिल तड़प रहा था चैन मिला, कब क्या हो जाये ख़ुदा जाने ॥
बाखुदी का जंगल ख़ाक हुआ, ज़ालिम थे जानवर भाग गये ।
मिल गई हुकूमत आज़ादी, कब क्या हो जाये ख़ुदा जाने ।।
मैकदा न जाकर जाम पीया, सिजदा न किया बुतखाने का ।।
फिर भी ये बेहोशी आ टपकी, कब क्या हो जाये ख़ुदा जाने ।।
खुद के घर में आबाद हुआ, दुनियाँ का पर्दाफाश हुआ ।
हो गये अलविदा आँख-कान, कब क्या हो जाये ख़ुदा जाने ।।
'मैं' कौन हूँ, जुर्रत है किसकी, महफिल में जो कर सके बयाँ ॥
ये जुर्म है सरेआम 'मुक्ता' कब क्या हो जाये ख़ुदा जाने ॥
जो पुरुष है, वह पुरुष होते हुए प्रसिद्ध है, प्रकाशनिधि है, प्रगट है और परावरन
है।
'परावरनाथ' परा माने माया, अवर माने संसार (वर माने श्रेष्ठ, अ, माने नई अर्थात् जो श्रेष्ठ न हो, उसको कहते हैं - संसार। अपने आप 'मैं' आत्मा अस्तित्व स पहले देह माना यह है माया, इसके बाद देह मानकर फिर स्त्री, पुरुष। बालक, युट वृद्ध। माता-पिता, भाई-बहिन आदि माना यह मान्यता हुई, यह है संसारा
माया और संसार का जो नाथ है, आधार है 'मैं' आत्मा, वह है परावरनाथ।
'मैं' आत्मा, आधार को खिसका लो, तो न माया रह सकती है और न संसार हूं रह सकता है। ये दोनों किसके आधार पर रहेंगे? टिकेंगे किस पर? इसलिए मैं आत्मा माया और संसार (परा और अवर) दोनों का आधार (नाथ) परावर नार हुआ।
निज भ्रम नहिं समुझहिं अग्यानी। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी ।।
भैया! जीव का स्वभाव होता है कि वह अपनी परछाई दूसरों पर देखता है किसी महात्मा के पास, चार व्यक्ति गये, तब उनमें से एक व्यक्ति ने महात्मा के देखकर, अपने साथियों से कहा- अरे, यह तो चोर है, हमने इसे चोरी करते देखा। और यह यहाँ महात्मापने का ढोंग लगाये बैठा है।
दूसरे ने कहा अरे! यह तो शराबी है, हमने इसे शराब पीते देखा है।
तीसरे ने कहा- अरे, यह तो व्यभिचारी है, हमने इसे वेश्या के कोठे पर देख
चौथे ने कहा- अरे, यह तो जुवाड़ी है, हमने इसे जुवा खेलते देखा है।
महात्मा, प्रत्येक की बात सुनकर कहते गये, हाँ भैय्या! तुम ठीक कहते है इसके बाद वे चारों वहाँ से चल दिये, तब वहाँ पाँचवा व्यक्ति जो पहले से महात्मा पास बैठा था, महात्मा से कहने लगा, भगवन्! आपने सब को, "हाँ भैय्या ठी कहते हो" । ऐसा क्यों कहा?
महात्मा ने कहा भाई! जो जैसा होता है, अन्य को वह वैसा ही देखता औ समझता है।
जीव का स्वभाव है कि अपनी परछाई वह दूसरों पर देखता है, वह दोष रवयं मे रहता है, इसलिए उसे वह दोष दूसरों में दीख पड़ता है।
जो जैसा है, वैसा ही परमात्मा को देखता है। ब्रह्मवादी की दृष्टि में सारा संसार आत्मा है, राम है और जीवनैष्ठिक की दृष्टि में सारा संसार जीव ही जीव दिखता है, देहाभिमानी की दृष्टि में सारा विश्व देहाभिमानी की ही दृष्टि में देखा जाता है। इस को तरह जो जैसा है, उसे सब वैसे ही दिखते हैं।
जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ।।
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ।।
सूर्य और आँख के बीच बादल के आ जाने पर सूर्य दिखाई नहीं देता, जिसे ही अज्ञानी समझता है कि बादल ने सूर्य को ढाँक लिया। कहो, इतने बड़े सूर्य को क्या बादल ढाँक सकता है? नहीं। पर अज्ञानी ऐसा कहता है कि बादल ने सूर्य को ढाँक लिया, वह यह नहीं जानता कि सूर्य और आँख के बीच बादल के आ जाने से सूर्य नहीं दिख रहा है। इसी तरह जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसको चन्द्रमा दो दिखाई देता है, यद्यपि चन्द्रमा दो नहीं, एक ही है।
उमा राम विषइक अस मोहा। नभ तम घूम घूरि जिमि सोहा ।।
(उ माने तप, मा माने मत करो, अर्थात उमा माने अब तपस्या मत करो। उस को दिन से उमा नाम पड़ गया) इस तरह राम में जो दोष दिखाई देता है वह अपना दोष है है। राम तो जैसा है, वैसा ही है। राम के विषय में अज्ञानवश कुछ भी कहना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुँआ और धूलि है कहना। आकाश तो नित्य, निर्मल और निर्लेप है, ये उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकते।
विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता ।।
विषय पाँच हैं- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधा करन माने इन्द्रिय।
शब्द विषय का कर्ण इन्द्रिय है, रूप विषय का चक्षु इन्द्रिय है, रस का जिह्ना, गंध का घ्राण और स्पर्श का त्वचा इन्द्रिय है। इन्द्रियों के जो देवता हैं, उन्हें कहते हैं के सुरजीव।
भैय्या! जीव जगत् बड़ा विशाल है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को छोड़कर जितने देवता हैं, ये सब जीव ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ईश्वर कोटि के देवता हैं।
कर्ण इन्द्रिय का देवता दिशा, नेत्र इन्द्रिय का देवता सूर्य, घाण इन्द्रिय का देवता अश्विनीकुमार, मन का देवता चन्द्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, अहंकार का देवता शंकर, चित्त का देवता नारायण, पैर का उपेन्द्र अर्थात् वामन भगवान, भुजा का इन्द्र इत्यादि से सब देवता एक से एक सचेत और बड़े चतुर हैं।
देखो-नेत्र का देवता सूर्य है। शरीर के सब अंगों में ठंड का असर होगा, परन्न आँख को ठण्ड नहीं लगती। कितनी ही बर्फीली जगह में चले जाओ अथवा पूस की कड़ाके की ठण्ड क्यों न हो पर आँख को ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि आँख का देवता सूर्य जो है। सूर्य में ठंडक का क्या काम? वाणी का देवता अग्नि है। मुँह में पान भरकर बोलो, क्या बोल सकते हो? नहीं। क्योंकि पानी और अग्नि की दुश्मनी है इसलिए जीभ हमेशा गीली रहती है, कभी सूखती ही नहीं। पैर का उपेन्द्र है। पैर में वामन भगवान निवास करते हैं इसलिए जब कभी भी किसी की पूजा होती है तो पैर की पूजा होती है। सिर की पूजा कोई नहीं करता, क्योंकि पूजा वामन भगवान की होती है। ये सब इन्द्रियाँ एक दूसरे के सेवक हैं। इन सबों में बड़ी एकता है। अपनी- अपनी ड्यूटी सब पूरा करते हैं।
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥
कान के सुनने और नहीं सुनने, आँख के देखने और नहीं देखने, मन के मन और अमनन, चित्त के चिन्तन और अचिन्तन, बुद्धि के निश्चय और अनिश्चय इन् सबको 'मैं' आत्मा ही जानता हूँ। इनका परम प्रकाशक हूँ, परम ज्ञाता हूँ, इसलिए 'सबकर परम प्रकाशक' 'मैं' आत्मा ही हुआ। बिना बोधवान विद्वान के एक बिना सन्त कृपा के ये बातें समझ में नहीं आती।
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ग्यान गुन धामू ।।
प्रकाश्य अर्थात् ज्ञेय। प्रकाशक अर्थात् ज्ञाता। जगत् मेरा दृश्य है और 'मैं' आम इसका दृष्टा हूँ। 'मैं' आत्मा मायाधीश हूँ। माया का ईश अर्थात् माया का आधार है कारण हूँ और ज्ञान तथा गुणों का भण्डार हूँ। 'मैं' आत्मा क्या नहीं जानता?
जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया ।।
जिसकी सत्यता करके माया जड़ होते हुए भी सत्य-सा भासती है। माया अर्थात मान्यता। माया, किसकी सहायता से सत्य-सा भासती है? "मोह सहाया" अर्थात अज्ञान की सहायता से सत्य-सा भासती है कैसे?
देखो - अंधेरे में जो सर्प दिखा, कौन सर्प दिखा? रस्सी! तब सर्प में जो सत्यत है वह सर्प की है या रज्जू की है?
उत्तर-रज्जू अर्थात् रस्सी की है, क्योंकि रज्जू ही तो है। सर्प न तो अंधेरे में है, न उजाले में। सर्प तो है ही नहीं, असत्य है। सर्प ही माया है, जो है ही नहीं।
उसी प्रकार माया में जो सत्यता है, वह सत्यता माया की है या राम की? राम की है। सत्य इव माने सत्य के समान। भगवान आत्मा में जो माया दिखती है वह सत्य नहीं, सत्य इव अर्थात् सत्य के समान है। रस्सी सर्प के रूप में क्यों दिखी? दिखने का क्या कारण है? अंधकार। इसी तरह भगवान आत्मा के अज्ञान में माया दिखती है? "मोह सहाया"। भगवान आत्मा 'मैं' का जिसको अज्ञान है, उसको ही भगवान माया के रूप में दिखाई देता है। तब भगवान ही माया है। केवल ज्ञान और अज्ञान का ही सवाल है। ज्ञान यही है कि सर्प को रस्सी से भिन्न मत मानो, सर्प को रस्सी ही जानो। ऐसे ही माया को भगवान से भिन्न मत मानो, माया को भगवान ही जानो। जो माया को भगवान से भिन्न मानते हैं, उसे माया चक्कर में डालती है, पेरती है, मरोड़ती है। यही माया में दोष है और जो माया को भगवान ही जानते हैं, उसे माया भगवान का दर्शन कराती है। यही माया का गुण है।
व्यवहारिक जगत् में देखो अगर किसी साहब से मिलना हो तो सहबिन को खुश कर लो, उनसे मिल लो, उनसे मिलने पर यदि वह खुश हो गयी तो साहब के मिलने से खुश होने में क्या देर सब काम बन जाते हैं, तब जगन्नियन्ता अखिल ब्रह्माण्ड के नायक चराचर के स्वामी, जो साहब हैं, उसकी जो सहबिन माया है, उसको खुश कर लो, फिर दर्शन में क्या देर है वह खुद दर्शन करा देगी।
प्रश्न- इस सहबिन को कैसे खुश किया जाय?
उत्तर-अरे, उसको साहब से भिन्न मत मानो, उसको साहब ही जानो, यही उसके खुश करने का तरीका है।
वृन्दावन में जाकर देखो, वहाँ पर जहाँ जाओगे, वहीं सबके सबको जय राधे- जय राधे ही पुकारते पाओगे, उनका कहना है कि राधा के वश में भगवान हैं, इसलिए राधा को जहाँ हमने खुश कर लिया कि भगवान श्रीकृष्ण खुश हुए ही हैं। उनके खुश होने में फिर क्या देर है।
बाबा के दरबार में, बाई कहैं सो होय ।।
भैया! यहाँ तक तो ब्रह्म का निरूपण हुआ, अब इधर जगत् का निरूपण है।
दोहा-
रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानुकर बारि ।
जदपि मृषा तिहुँ काल, सोई भ्रम न सकइ कोउ टारि ।।117।।
जैसे सीप में चांदी का भ्रम, सूर्य की किरणों में मृगतृष्णा के जल का भ्रम, ट्रॅट म पिशाच का भ्रम और रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, परन्तु ये सब भ्रम, मिथ्या और असत्य है।
उसी प्रकार -
एहि बिधि, जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई ।।
'मैं' आत्मा के आधार पर जगत प्रपंच, मिथ्या, असत्य और दुःख रूप है। मिथ्या और असत्य में अन्तर है, उत्पन्न होकर जो नाश हो जाये वह है मिथ्या और जो तीनों काल में न हो, बन्ध्या पुत्रवत्, वह असत्य है।
शरीर देश में शरीर मिथ्या है और आत्मदेश में, भगवान देश में, शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं है, अतः शरीर असत्य है। संसार या माया, इसी प्रकार 'मैं' आत्म देश में है ही नहीं, जैसे मृगजल में जल नहीं है, सीप में चांदी नहीं है, दूँठ में पिचाश नहीं है और रस्सी में सर्प नहीं है परन्तु -
जदपि असत्य देत दुख अहई ।।
वह नहीं होते हुए भी दुःख का कारण बना है। दुःख दे रहा है इस दुःख का कारण भ्रम है। नहीं होते हुए भी उसे सत्य मान लेना ही दुःख का कारण है।
जौं सपने सिर काटै कोई। बिनु जागे न दूरि दुख होई ।।
जैसे स्वप्न में अपना सिर कटा हुआ दिखा, भला जिसका सिर कट जायेगा, वह अपने कटे हुए सिर को देख सकता है? नहीं, पर दिखा और इस दुःख से वह बहुत व्याकुल है, तो इस दुःख से छुटकारा तो जागने पर ही मिल सकेगा, बिना जागे दुःख का अन्त, किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'मैं' स्वस्वरूप भगवान आत्मा में बिना जागे इस भ्रम का निवारण नहीं हो सकता और जब तक यह भ्रम हटेगा नहीं तब तक इस महान विपत्ति से छुटकारा नहीं मिल सकता।
सन्त तुलसीदास जी विनय में कहते हैं -
हे हरि! यह भ्रम की अधिकाई ।
देखत, सुनत, कहत, समुझत, संसय-संदेह न जाई ।।
हे हरि! यह भ्रम की अधिकता है कि देखने, सुनने, कहने और समझने पर भी, न तो संशय ही जाता है और न सन्देह ही दूर होता है।
संशय, यह कि असत्य जगत् को सत्य मानना और सन्देह यह कि एक परमात्मा की ही अखण्ड सत्ता है या कुछ और भी है।
जो जग मृषा, ताप त्रय अनुभव, होइ कहहु केहि लेखे ।
कहि न जाय, मृगबारि सत्य, भ्रम ते दुख होइ बिसेखे ||2||
कोई कहे कि संसार असत्य है तो संसार के ताप भी असत्य हैं, परन्तु तापों का अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है?
तो भैय्या! इसका उत्तर यह है कि मृगतृष्णा का जल सत्य नहीं है, परन्तु जब तक भ्रम है, तब तक वह सत्य ही दिखता है और उसी भ्रम के कारण अज्ञानी मृगों को विशेष दुःख होता है। इसी प्रकार जगत् में भी भ्रमवश दुःखों का अनुभव होता है।
सुभग, सेज, सोवत सपने, बारिधि बूड़त भय लागै ।
कोटिहुँ नाव न पार पाव सो, जब लगि आपु न जागै ।।३।।
जैसे, कोई सुन्दर सेज पर सोया हुआ मनुष्य सपने में समुद्र में डूबने से भयभीत हो रहा हो, पर जब तक वह स्वयं जाग नहीं जाता, तब तक करोड़ों नौकाओं द्वारा भी वह पार नहीं जा सकता। उसी प्रकार यह जीव, अज्ञान निद्रा में अचेत हुआ, संसार सागर में डूब रहा है तो वह स्वस्वरूप भगवान आत्मा में बिना जागे, सहस्त्रों साधनों द्वारा भी दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता।
अनबिचार रमनीय सदा, संसार, भयंकर भारी ।
सम संतोष, दया बिवेक तें, व्यवहारी सुखकारी ।।4।।
यह अत्यन्त भयानक संसार अनविचार से ही पैदा हुआ, अज्ञान के कारण ही मनोरम दिखाई देता है, यह उनके लिए ही सुखकारी है, जिनने अपने स्वरूप भगवान आत्मा को जान लिया है। संसार अनविचार से किस तरह पैदा होता है, इस पर एक दृष्टान्त सुनो - -
एक भागवती पण्डित किसी दूसरे गाँव को भागवत की कथा कहने गया। उसने निस्तार के लिए अपने साथ दो लोटा रख लिया। मार्ग में उसे एक नदी मिली। उसने सोचा कि यहाँ स्नान कर लें, फिर आगे बढ़ें। नदी में स्नान करते समय पंडित जी ने सोचा कि वहाँ दो-दो लोटा ले जाकर क्या करूँगा, मुझे साथ में एक लोटा लेकर चलना था। अरे! जहाँ जाऊँगा, लोग वहाँ लोटे का प्रबंध तो कर ही देंगे। मुझे अपने साथ एक ही लोटा रख लेना पर्याप्त है। दो-दो लोटा रखने में चोरी हो जाने का भी भय है। ऐसा सोचकर उसने एक ही लोटा ले चलने का निश्चय किया। पण्डितजी ने नही में स्नान किया और एक लोटा को वहीं नदी की रेत में गड्ढा बनाकर छिपा दिया। उसने सोचा कि लौटते वक्त तो इसी मार्ग से ही लौटना है, उस समय लोटा निकाल कर लेता जाऊँगा। लोटे को छिपाने के स्थान को भूल न जाऊँ इस विचार से पहचान के लिए उसने वहीं रेत का मीनार बना दिया और वहाँ से चल दिया। वहाँ से कुछ ही दूरी पर नदी में जो लोग स्नान कर रहे थे, उन लोगों ने पण्डितजी को लोटा गड़ाते तला नहीं देखा, परन्तु मीनार बनाते हुए देख लिया। लोगों ने सोचा कि आज कोई न कोई महान् पर्व है, इस पर्व में स्नान करने के बाद रेत में मीनार बनाने का महत्व है, तभी तो पण्डितजी महाराज ने स्नान करके मीनार बनाया है। बस, फिर क्या था सब लोग स्नान कर करके रेत में मीनार बनाते गये और अपने-अपने घर की ओर रवाना हुए। इस तरह नदी में वहाँ पर लोगों के द्वारा सैकड़ों मीनारें बन गयी।
जब पण्डित जी महाराज कथा समाप्त करके वापस लौटे, तब अपना लोटा निकाल लेने के लिए वे नदी में गये। वहाँ पहुँचकर पण्डितजी ने देखा कि नदी के रेत में सैकड़ों मीनारें बनी हुई हैं। इन मीनारों में पण्डितजी की बनायी हुई मीनार खो गयी। वे अचम्भे में पड़ गये और यह निश्चय नहीं कर सके कि इन मीनारों में उनकी बनाई हुई मीनार कौन-सी है? उन्होंने घंटे भर तक पच्चीस-तीस मीनारों में अपना लोटा ढूँढा, परन्तु उन्हें लोटा न मिला। लाचार हो, उदास चित्त अपने गाँव को चल दिये।
भाई! देखो-संसार, हानि-लाभ और बिना अर्थ को समझे औरों की देखा-देखी ही करता है। बिना अर्थ किये, मीनारों का संसार बस गया। इस संसार की रचना, अनविचार से ही हुई। संसार, अनविचार से ही पैदा होता है।
तुलसिदास, सब बिधि, प्रपंच जग, जदपि झूठ, श्रुति गावै ।
रघुपति भगति, सन्त संगति बिनु, को भव त्रास नसावै ।।
(विनय पत्रिका 121)
मानसकार कहते हैं कि वेद कह रहे हैं, यद्यपि सांसारिक प्रपंच सब प्रकार के असत्य हैं, किन्तु रघुनाथजी की भक्ति और सन्तों की संगति के बिना इस संसार के भीषण भय का नाश नहीं हो सकता और न इस भ्रम का ही निवारण हो सकता है।
जासु कृपाँ अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ।।
'मैं' आत्मा को ही मैंने माया, संसार मान लिया है, यह जब तक न जाना जायेगा, तब तक दुःख है। 'मैं' आत्मा की ही कृपा से 'मैं' का ज्ञान होता है, इस 'मैं' को जानो, फिर माया और संसार नहीं और जब माया और संसार नहीं रहा, तब उससे उत्पन्न हुआ दुःख नहीं। जिस भगवान आत्मा 'मैं' की कृपा से, इस भ्रम का निवारण होता है,
गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ।।
प्रश्न होता है, यह कैसा है -
आदि अन्त कोउ जासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा ।।
वह आदि, अन्त और मध्य से रहित है।
वेद, शास्त्र, श्रुति आदि भी जिसको नहीं जान सके, उन्होंने केवल अपना- अपना अनुमान ही बताया।
उसकी महिमा इस प्रकार है -
बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ बिधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी ।।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहइ घान बिनु बास असेषा ।
असि सब भाँति, अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ।।
दोहा-
जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि घरहिं मुनि ध्यान ।
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ।।118।।
राम सो परमातमा भवानी। तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी ।।
हे पार्वती वही परमात्मा श्री रामचन्द्र जी हैं। उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम का होना अनिष्टकारक है।
अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं ।।
इसमें भ्रम जहाँ हुआ कि मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सभी गुण नष्ट हो जाते हैं।
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटिगै सब कुतरक कै रचना ।।
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दारुन असंभावना बीती ।।
भगवान शंकर के इन भ्रम नाशक वचनों को सुनकर, माताजी के सब संशय ना हो गये। उनके मन में जो असम्भावना थी कि -
जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि ।।
दशरथ सुत राम, कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकते यह जाता रहा और भगवत चरणे में उनकी दृढ़ निष्ठा हो गयी।
बस, यहीं पर शंकर-गीता का उपसंहार है।
रामु अमित गुन सागर, थाह कि पावइ कोइ ।
संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ, तुम्हहिं सुनायउँ सोइ ॥
॥ॐ श्री सदगुरु देवाय नमः ।।
श्री रामचन्द्राय नमः
श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस
बालकाण्डान्तर्गत
2. राम नाम महिमा
मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम् ।
यत्कृपातमहं बंदे परमानंद माधवम् ।।
चौपाई -
बंदउँ राम नाम रघुबर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ।
बिधि हरिहर मय बेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान से ।।
मैं श्री रघुनाथजी के राम नाम की वंदना करता हूँ कि जो कृशानु (अग्नि) भानु (सूर्य) और हिमकर (चंद्रमा) का कारण है तथा उनका शक्तिदाता है। राम के प्रताप से ही ये तीनों तेजस्वी, प्रकाशवान व ज्योतिर्मान हुए हैं। राम नाम के एक-एक अक्षर से ये तीनों शक्ति प्राप्त किये हैं। यदि कृषानु में से 'र', भानु में से 'अ' और हिमकर में से 'म' निकाल लिया जाये तो तीनों ‘र+ आ + म ‘अर्थात् राम निकल जाने से वे शक्तिहीन और निरर्थक हो जाते हैं। कृशानु में से 'र' निकल जाने से कशानु रह जाता है, जो अग्नि का द्योतक न होने से उष्णताहीन और जलाने की शक्ति से रहित है। भानु में से 'अ' निकल जाने से सिर्फ भनु रह जाता है, जो सूर्य का प्रतीक न होने से प्रकाश देने की शक्ति से रहित हो जाता है। उसी प्रकार हिमकर में से 'म' के निकल जाने पर केवल हिकर रह जाता है, जो चंद्रमा का प्रतीक न होने के कारण शीतलता व शांति प्रदान नहीं कर सकता। इस तरह राम अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण है, प्राण है, बीज है।
'तत्त्वमसि' सामवेद का महावाक्य है जो जीव व ब्रह्म की एकता का समर्थक है। तत् त्वम् का अर्थ है-वह तू है। तत् पदवाची रा और त्वम् पदवाची म् का संयोग होने से असि पदवाची राम हो जाता है। असि माने 'है' होता है। इस तरह वह 'है' ही है जो राम है। 'है' अर्थात् अस्तित्व, वही 'है', वही राम, अग्नि, सूर्य व चंद्रमा का कारण है, बीज रूप है। वह प्रणव यानी ऊँ (ओंकार) का भी बीज है।
राम नाम के तीनों अक्षर र अ म क्रमशः कृशानु, भानु और हिमकर के बीजाक्षर हैं, र अग्नि बीज है, अ भानुबीज और म चंद्रबीज है। जैसे अग्नि शुभाशुभ वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देता है और कुछ वस्तुओं का मल और दोष जलाकर उनको स शुद्ध कर देता है, वैसे ही 'र' के उच्चारण से मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मनाश हो जाते हैं और मन का विषयवासना रूपी मल जलकर भस्म हो जाता है। भानुबीज 'अ' वेदशास्त्रों के प्रकाशक है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही 'अ' से अज्ञानरूपी अंधकार का नाश होकर ज्ञान का प्रकाश होता है। चंद्रबीज में 'म' अमृत से परिपूर्ण है। जैसे चंद्रमा ताप को हरता है और शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही 'म' से हृदय में भक्ति का उदय होता है जो त्रिताप को हरता है तथा शीतलता और शांति प्रदान करता है। सारांश, राम नाम के स्मरण से वैराग्य, ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। सब शुभाशुभ कर्मों तथा अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है, हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होकर ज्ञान का प्रकाश होता है और तीनों तापों का नाश होकर परम शांति प्राप्त होती है।
दूसरा भाव यह है कि जगत् प्रसिद्ध तीन राम हुए हैं- परशुराम, राम और बलरामा अग्निवंश में परशुराम, सूर्यवंश में राम और चंद्रवंश में बलराम। यदि इन वंशों में से राम निकाल दिये जायें तो ये वंश भी अन्य वंशों की भाँति ख्यातिहीन हो जायेंगे और विस्मृति के गर्त में डूब जायेंगे।
बिधि हरिहर मय वेदप्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो ।।
यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है तथा वेदों का प्राण ऊँ (ओंकार) है। फिर भी वह गुणों से रहित व अनुपमेय होने के साथ-साथ गुणों का भण्डार है।
यह राम नाम कैसा है? यह 'र' यानि रकार से विधिरूप अर्थात् ब्रह्मारूप है, 'अ' यानि आकार से हरिमय अर्थात् विष्णु रूप है और म यानि मकार से हरमय अर्थात् शंकर रूप है। इस तरह राम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है। तात्पर्य, भगवान राम देवों के देव और वेदों के प्राण ऊँ (ओंकार) हैं। ओंकार के अउम में 'अ' हरिवाचक, 'उ' विधि वाचक और 'म' हरवाचक है। इस तरह ऊँ (ओंकार) भी विधि-हरि-हर मय है। फिर यह राम का नाम तीनों गुणों से यानि सत्, रज, तम से परे है। तीनों गुणों से रचा हुआ जो यह जगत् प्रपंच है, उससे राम अलिप्त है, क्योंकि वह (राम) निराकार है, निर्विकार व असंग है। फिर राम एक है, सत् चित् आनंद है और मन, वाणी, बुद्धि से परे है। मन वाणी से परे होने के कारण भगवान राम अनिवर्चनीय है, इसलिए उसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। वह सर्वथा अनुपमेय है। तीनों गुणों से रहित होते हुए भी भगवाम राम के नाम का जप व स्मरण सब सिद्धियों का दाता है। इस तरह राम का नाम सब गुणों का भण्डार है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो राम नाम के प्रताप से प्राप्त न हो सके।
राम यह वेदों का प्राण है, क्योंकि वेद का मूल जो ओंकार है, वह राम नाम से ही निकला है। यथा -
स्वांसा में सोहम् हुआ, सोहम् में ओंकार ।
ओंकार से रर्रा हुआ, साधो करो विचार ।।
ऊँ (ओम) शब्द आत्मा का बोधक है। ओंकार का अ उ म और मात्रा अनुस्वार अस्तित्व का रूप राम का द्योतक है। यह अस्तित्व रूप राम अर्द्धमात्रा रूप से नित्य स्थित है और उसका कभी नाश नहीं होता। उसे चाहे शक्ति कहो, चाहे शक्ति का आधार कहो, आत्मा कहो, चाहे राम कहो, चाहे जो कहो सब एक ही है। वह अर्द्धमात्रा वाणी से परे है और वही ओंकार है, जो राम नाम से निकला है।
महामंत्र जेई जपत महेसू । कासी मुकुति हेतु उपदेसू ।।
भगवान राम का नाम महामंत्र है, जो सब मंत्रों में श्रेष्ठ है और जिसे शंकर जी हमेशा जपते रहते हैं। शंकर जी द्वारा उस महामंत्र का उपदेश काशी में मरने वाले लोगों के लिए उनके मुक्ति का कारण होता है।
काशी का अर्थ है-"काशः ब्रह्मप्रकाशः यस्यां अवस्थायां सा काशी।" अर्थात् जिस अवस्था में ब्रह्म का प्रकाश हो यानि आत्म अनुभव हो, उसे कहते हैं काशी। भाव यह है कि राम नाम के माध्यम से शंकर जी काशी में निवास करने वाले लोगों को आत्मतत्त्व का उपदेश करते हैं और जब उन लोगों को आत्म अनुभव हो जाता है, तब स्वरूप में विभोर रहने वाले प्राणी जीते जी मर कर मुक्त हो जाते हैं। जीव भाव का अभाव होना और आत्म भाव का जागृत होना ही जीते जी मरना है। आत्म भाव के प्राप्त होने पर जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है और यही उसका काशी में मुक्ति है।
महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥
उस राम नाम की महिमा को गणों के अधिपति गणेशजी भली भाँति जानते थे और इसीलिए उस राम नाम के प्रभाव से वे अग्रपूज्य हो गये और सब मांगलिक कार्यों में सब देवों की अपेक्षा उनकी पूजा सर्वप्रथम होने लगी।
'गणराऊ' का अर्थ होता है गणों का राजा, गणों का पति, गणों का ईश अर्थात गणपति या गणेश। 'गण' शब्द समूह का वाचक है। समूहों के रक्षक, समूहों के पालन करने वाले परमात्मा को गणपति कहते हैं। सम्पूर्ण दृश्य मात्र का जो अधिष्ठान है, इंद्रिय गणों का जो संचालक है, वही गणपति है। इस प्रकार अस्तित्व रूप, सर्वाधार सर्वव्यापक, देवाधिदेव, परात्पर ब्रह्म भगवान आत्मा राम ही गणेश या गणपति है। शिव-पार्वती-पुत्र गणेशजी उन गणाधिपति देवाधिदेव सनातन ब्रह्म भगवान राम के प्रतीक हैं और चूँकि वे राम की महिमा को जानते थे, इसलिए उनके माध्यम से ऊ अनादिदेव भगवान राम का पूजन सर्वमंगल कार्यों के आरम्भ में सर्वप्रथम किया जाता है।
एक बार देवों में विवाद खड़ा हो गया कि सब में अग्रगण्य या अग्रपूज्य कौन है? ब्रह्माजी की सभा में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा करने जो सर्वप्रथम आयेगा, वही सब में अग्रपूज्य होगा। सब देवतागण अपने-अपने शीघ्रगामी वाहनों पर चढ़कर दौड़ चले। गणेशजी का वाहन मूषक धीमी गति वाला था और इसीलिए वे सबसे पीछे रह गये। रास्ते में उनको नारद जी मिले। नारद जी के उपदेश पर उनको राम की महिमा का ज्ञान हुआ और वे राम का नाम पृथ्वी पर लिखकर उसकी प्रदक्षिणा कर सर्वप्रथम ब्रह्माजी के पास पहुँच गये और इस कारण वे सबसे अग्रपूज्य बनाये गये। यह है राम के नाम की महिमा और गणेशजी के अग्रपूज्य होने का रहस्य।
श्रीगणेशजी के अग्रपूज्य होने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। उनके श्री विग्रह का एक मुख्य भाग यानि मुख गजमुख है जो एकाक्षर परब्रह्म रूप ओंकार (ॐ) का ही प्रतीक है। उनके सूंड सहित गज-आनन को देखकर (ॐ) ओंकार का स्पष्ट रूप से आभास मिलता है। ओंकार सृष्टि का आदिबीज और अव्यक्त परब्रह्म का व्यक्त स्वरूप है। ओंकार और परब्रह्म का वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। श्रीगणेशजी परन मंगल स्वरूप सर्वाधार आदिदेव ओंकार परब्रह्म ही हैं। वे श्रीराम रूप ही हैं। अतः उनका सर्वाग्र पूज्य होना उचित एवं स्वभाविक है और उनके विशिष्ट अधिकार का मूल कारण है।
जान आदि कवि नाम प्रतापू। भयउ सिद्ध करि उल्टा जापू ।।
भगवान राम के नाम के महत्व को ऋषि प्रवर आदि कवि वाल्मीकि जी जान गय क्योंकि उस नाम के उल्टा जाप से भी वे सिद्धता को प्राप्त हो गये।
वाल्मीकि जी राम नाम का जप निरंतर, अटूट गति से करते थे। जप अटूट होने से राम का उच्चारण रा मरा मरा मरा मरा मरा म होने लगा। वे जप में इतने तन्मय हो गये कि उन्हें किसी बात की सुधि नहीं रही। उनकी मनोवृत्ति सांसारिक विषयों से उलट कर आत्मिक या ब्रह्ममय हो गयी। ऋषिराज ने नाम का जप साधारण जीभ से न कर छोटी जीभ से, जो कंठ के भीतर रहती है और जिसको कौआ या अंतर्जीभी कहते हैं, किया। फलस्वरूप उनकी वृत्ति संसार से उलटकर तत्काल अंतर्मुखी हो गयी और वे निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो गये। वे जप में या तपस्या में इतने लवलीन हो गये कि उन्हें तन-वदन की सुधि नहीं रही और उनके शरीर पर वल्मीक जम गयी। उनकी दृष्टि में संसार रह ही नहीं गया। उनके लिए सर्वत्र केवल आत्मा- राम ही था, राम के अतिरिक्त कहीं कुछ था ही नहीं। इस प्रकार वृत्ति को उलटकर जप करके वाल्मीकि जी सिद्ध हो गये तथा भूत भविष्य का ज्ञान, उनके लिए हस्तामलक वत् हो गया और उन्होंने रामायण के रचनाकर आदि कवि होने का यशोपार्जन किया।
सहसनाम सम सुनि सिव बानी। जपि जेई पिय संग भवानी ।।
हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को ।।
नाम प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को ।।
भगवान राम का नाम एक बार लेना विष्णु के सहस्त्र बार नाम जपने के बराबर है-ऐसा शिवजी का वचन सुनकर पार्वती जी राम नाम जपकर महादेवजी के साथ भोजन करने बैठी। राम नाम के प्रति पार्वतीजी की प्रीति, निष्ठा व विश्वास तथा अपने वचनों पर उनकी अटूट श्रद्धा देखकर शिवजी ने उन्हें पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि कर दिया और अपने अंग का भी भूषण अर्थात् अर्धांगिनी बना दिया। राम नाम की महिमा को स्वयं शंकर जी अच्छी तरह से जानते हैं और उसी के प्रभाव से हलाहल भी उन्हें अमृत का सा फल दिया।
अब यहाँ प्रश्न होता है कि विष क्योंकर अमृत तुल्य हुआ ? भगवान शिव निरंतर श्रीराम नाम का जप करते रहते हैं। जप में वे इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें भगवान राम के अतिरिक्त कुछ दूसरा दिखता ही नहीं। वे सर्वदा निर्विकल्पावस्था में अर्थात् स्वरूपस्थ रहते हैं। उनकी दृष्टि में न तो संसार है और न प्रपंच जनित कोई अन्य पदार्थ। उनकी दृष्टि में न तो विष है और न अमृत। उनकी धारणा में सब कुछ राम है। अतः, जो पदार्थ संसार वालों की नजर में यानि जीववादियों की दृष्टि में विष था, वह शंकर जी की दृष्टि में राम था, राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। राम अपना आप अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप यानि स्व-स्वरूप किसी को भी अहितकारी न होता। वह सर्वदा सर्वरूपेण हितकारी या कल्याणकारी होता है। अतः, शंकरजी क हलाहल विष भी अमृत तुल्य फल दिया।
दोहा -
बरषा रितु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास ।
राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास ।। 18।।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति तो वर्षा ऋतु है, श्रो भक्तजन धान की फसल हैं और राम के नाम के दोनों सुंदर अक्षर रा और म श्रावा और भादों महीनें हैं।
जिस तरह श्रावण और भादों के महीनों में अच्छी वर्षा होने से धान की फसल के बाढ़ अच्छी होती है, उसी तरह राम नाम के दोनों अक्षरों को अच्छी तरह से हृदयः धारण करने से यानि उनके निरंतर जप से भक्तों के हृदय में भक्ति की वृद्धि होती और उनका सब प्रकार से कल्याण होता है। वे कृतकृत्य हो जाते हैं।
आखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन बिलोचन जन जिय जोऊ ।
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहु परलोक निबाहू ।।
राम नाम के दोनों अक्षर 'र' और 'म' मधुर और मन के हरने वाले हैं, सब वणणे के नेत्र हैं अर्थात् सब अक्षरों के ऊपर शोभायमान होते हैं तथा भक्तजनों के जीवन और उनके हृदय को आलोकित करते हैं। उनका स्मरण सब कोई सरलतापूर्वक क सकते हैं, जो सबके लिए सुखदायक है और सब वस्तुओं के देने वाले हैं। उनका ज इस लोक में तो लाभकारक है ही, परलोक को भी सुधारने वाला है अर्थात् मोक्ष क सुलभ कर देता है।
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम पिय तुलसी के ।
बरनत बरण प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती ॥
ये दोनों अक्षर 'र' और 'म' कहने के लिए, सुनने में तथा जप करने के लि अति उत्तम हैं। राम शब्द का 'रा' राम-वाचक है और 'म' लक्ष्मण वाचक है। इसलि तुलसीदास के लिए राम और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इन दोनों अक्षरों को पृथक पृथक वर्ण का मानकर वर्णन करने में दोनों का अलग-अलग संबंध प्रतीत होता परन्तु, यथार्थ में ये दोनों ब्रह्म और जीव के सदृश एक हैं, अभिन्न हैं।
सरसरी तौर से ऊपर देखने पर 'र' और 'म' अलग-अलग वर्ण के प्रतीत होते हैं। 'र' य वर्ग और 'म' प वर्ग का है। 'र' मूर्द्ध संबंधी है और 'म' औष्ठ संबंधी। 'र' वैराग्यवाची है और म भक्तिवाची है। पुनः इनके वर्णन में न संग है और न प्रीति है। परन्तु, अर्थ में और लक्ष्य में संग और प्रीति दोनों है, क्योंकि 'रकार' ब्रह्म वाचक है और 'मकार' जीव वाचक है। जिस प्रकार ब्रह्म और जीव अलग-अलग न होकर एक ही हैं, उसी प्रकार 'र' और 'म' भिन्न-भिन्न न होकर एक भगवान राम को ही इंगित करते हैं।
जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, अभिन्न हैं। सनातन ब्रह्म भगवान राम सत्य हैं, अखण्ड और अद्वैत हैं। एक या अद्वैत वह है, जिससे भिन्न कोई दूसरा नहीं। एक वह है, जो सबका आधार है और जिसके बिना किसी अन्य की सिद्धि नहीं। भेद एक से अधिक में अर्थात् दो या दो से अधिक में होता है, एक में नहीं। इसलिए ब्रह्म (ईश्वर) में कोई भेद नहीं, वह अभेद रूप है। ब्रह्मा से आदि लेकर एक कण पर्यन्त सब ब्रह्म हैं, ब्रह्म से अभिन्न है। सारा चराचर ही ब्रह्म या ईश्वर है। फिर जीव, ब्रह्म से कैसे भिन्न होगा? इसलिए जीव भी ब्रह्म है। जीव व ब्रह्म में कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं, अभिन्न हैं। जो जीव है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही जीव है। दोनों में स्वाभाविक एकता या अभिन्नता है।
नर नारायन सरिस सुभ्राता । जग पालक बिसेषि जनत्राता ।
भगति सुतिय कल करन बिभूषण । जगहित हेतु बिमल बिधु पूषन ।।
ये दोनों अक्षर 'र' और 'म' नर व नारायण के समान प्रेमी भाई के सदृश हैं। ये संसार के पालन करने वाले हैं तथा भक्तजनों के विशेष रूप से रक्षक हैं। फिर ये दोनों अक्षर भक्ति रूपी सौभाग्यवती सुन्दर कामिनी के कानों के आभूषण हैं तथा संसार के कल्याण के मूल कारण व निर्मल पूर्ण चन्द्रमा के समान पोषक और शांतिदायक हैं।
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ सेष सम धर बसुधा के ।
जन मन मंजु कंज मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलधर से ।।
फिर, ये दोनों अक्षर सद्गति के देने वाले और अमृत के समान संतोषप्रद तथा अमरता प्रदान करने वाले हैं। ये कच्छप (कछुवा) तथा शेषनाग के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। फिर ये संतजनों के मन रूपी सुन्दर कमलों के लिए भौरों के समान हैं और जिह्वा रूपी यशोदा को श्रीकृष्ण व बलराम के समान प्रिय हैं।
जिस प्रकार अमृत अपनी अमरता प्रदान करने वाले गुण के कारण सर्वप्रिय अपनी संतोषदायक व आनंददायक स्वाद के लिए प्रशंसनीय है, उसी प्रकार ' और 'म' ये दोनों अक्षर सब जीवों के अत्यंत प्रिय, आनंद के दाता और सद्गति वरदाता हैं। जिस प्रकार पृथ्वी कच्छप और शेषनाग पर आधारित है, उसी तरह या समस्त जग प्रपंच रा + म अर्थात् राम पर आधारित है। राम ही समस्त चराचर क आधार है और उसका मूल कारण है। जिस प्रकार रस के लोभी भौरे कमल के सुन्दा फूलों पर गुंजारते व मंडराते रहते हैं, उसी तरह T + 7 भक्तों के निर्मल मन रूप कमलों में सदा रमण करते हैं। जिस प्रकार यशोदा मैया को कृष्णचन्द्र जी औ बलराम जी अत्यंत प्रिय थे और वे उनका नाम सदा ही लिया करती थी, उसी तरु 'रा' और 'म' यशोदारूपी जिह्वा के अत्यंत प्रिय हैं और उसके जरिये सदा जपे जार हैं। जिस प्रकार एक बालक के बिना घर की शोभा नहीं, उसी तरह मुख रूपी घरः जिह्वा रूपी माता की गोद में 'रा' और 'म' रूपी बालक न हो, तो मुख रूपी घर के शोभा नहीं। जैसे, यशोदा मैया को श्रीकृष्ण और बलराम प्रिय थे, वैसे ही भक्तों की जिह्वा को ये दोनों अक्षर अत्यंत प्रिय हैं। यशोदा जी जैसे सदा उनके लालन-पाल में लगी रहती थी, वैसे ही भक्त जापक जन इन अक्षरों को सदा ध्यान में रखते हैं औ स्मरण करते हैं ।।
एक छत्रु एकु मुकुटमनि, सब बरननि पर जोउ ।
तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दोउ ।।
तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दो अक्षरों में से रकार सब अक्षरों के ऊपर छत्र के समान और मकार मुकुट में मणि के समान अर्थात् बिन्दु के रूपः शोभित होते हैं। क्षत्र और मणि जडित मुकुट जिसके सिर पर होता है, वह राज कहलाता है। उसी तरह जो भक्त इन दोनों वर्णों को अपने हृदय के अन्दर धारण करते हैं, वे भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। वे जीवों की श्रेणी में न होकर राम (ब्रह्म) है हो जाते हैं। स्वरहीन होने से 'र' और 'म' सब वर्णों के ऊपर विराजते हैं। वैसे ही ज इनका अर्थात्, राम का अवलम्बन लेते हैं, वे भी (स्वरहीन) श्वाँस रहित होकर यान निर्विकल्पता को प्राप्त कर सद्गति पाते हैं।
समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ।।
नाम रूप दुई ईस उपाधी । अकथ अनादि सु सामुझि साधी ।।
समझने में नाम और नामी (नामधारी) एक समान हैं और उनका पारस्परिक प्रेम तथा संबंध स्वामी और सेवक के सदृश है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि अर्थात् माया हैं और इसीलिए अधिष्ठान आत्मा के सदृश अकथ और अनादि हैं तथा निर्मल व स्थिर बुद्धि से समझने व साधने योग्य है।
नाम और नामी (नाम वाला) अलग-अलग नहीं हो सकते, दोनो एक ही हैं। जिस प्रकार पुरुष से प्रकृति भिन्न नहीं, स्वभावी से स्वभाव भिन्न नहीं, उसी प्रकार नामी से नाम भिन्न नहीं, दोनों एक ही हैं। अध्यस्थ अधिष्ठान के अनुरूप रहता है, वैसे ही नाम नामी के अनुरूप होता है। जो गुण नामी में होते हैं, वे ही गुण नाम में भी होते हैं। भगवान में अनन्त गुण हैं और वे सभी गुण उनके नाम में भी हैं। नाम बीज है। बीज में कितना बड़ा वृक्ष समाया रहता है, वह बाद में तब दीखता है जब उस बीज से पेड़ तैयार होता है। जिस प्रकार बीज के अंदर सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप में पिंड़, डालियाँ, पत्ते, फूल, फल आदि विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार नाम में भी भगवान के समस्त गुण विद्यमान रहते हैं। नाम नामी से अभिन्न है। नाम ही भगवान है और भगवान ही नाम है।
उपाधि कहते हैं उपनाम को, जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ढाँकता है। जिसको जो ढाँके वही उसकी उपाधि है। जिस प्रकार उपाधि व्यक्तित्व को ढाँकती है, उसी प्रकार नाम और रूप भगवान के भगवानपने को ढाँकते हैं, इसलिए ये भगवान की उपाधि हैं, भगवान की माया हैं। भगवान की उपाधि है माया और भगवान है 'मैं' आत्मा। अपने आप में आत्मा को कुछ मान लेने से 'मैं' आत्मा उस मान्यता रूपी झाड़ी में छिप जाता है। यही भगवान के भगवान पने का ढक्कन है। मान्यता का त्याग यानि आत्म-ज्ञान की प्राप्ति, स्वरूप का बोध, मायापति भगवान आत्मा 'राम' का ज्ञान, यही मान्यता रूपी ढक्कन का उधरना है और माया का साधना है। माया का आधार मायापति को पहिचानना ही माया का समझना है तथा माया से तरना है।
प्रत्येक वस्तु में अस्ति, 'भाँति' प्रिय नाम और रूप से पाँच अंश विद्यमान रहते हैं। अस्ति माने हैं अस्तित्व अर्थात् सत्। भाति माने भासता है अर्थात् जो चेतन है, चित् है। प्रिय माने आनंद, आनन्ददायक, आनंदस्वरूप। अस्ति भाँति और प्रिय ये तीन भगवान आत्मा के बोधक हैं और नाम तथा रूप माया के द्योतक हैं। उदाहरण के लिए डंडा लीजिये। डंडा का अस्तित्व लकड़ी है, डंडा में जो भासता है वह लकड़ी है और डंडा में जो प्रियता है वह लकड़ी की है। उसी तरह शरीर को लीजिये। शरीर का जो अस्तित्व है यानि 'है' पना है, वह पंचमहाभूतों का है और पंच महाभूत सब भगवान आत्मा पर आधारित है। देह का जो भातिपना है वह चेतन का है यानि ' आत्मा का है। देह की जो प्रियता है, उसमें जो आनंद है, वह आनंद-स्वरूप 'b आत्मा का है। इसलिए शरीर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, जो कुछ शरीर रूप दिखाई दे रहा है, वह 'मैं' आत्मा ही है। 'मैं शरीर हैं' - ऐसा जो कहा जाता है, वह शरीर को मान कर कहा जाता है, जानकर नहीं। यदि शरीर को जानने (जाँचने चलो, तो देह मिलता ही नहीं। जो मिलता है वह है भगवान आत्मा 'मैं'। अर्थात् सर कुछ एक कण से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त समस्त चराचर भगवान आत्मा राम है। भगवान आत्मा राम के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं।
जगत् प्रपंच के अंदर जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह सब मान्यता है। वह मुड़ आत्मा को कुछ मानने पर ही दिखाई देता है और उसकी पहिचान के लिए उसक कुछ न कुछ नाम और रूप रहता है। अतः नाम और रूप विकल्प हैं, मान्यता है माया है यदि अस्ति भाँति प्रिय न हो तो नाम और रूप का आधार कौन होगा अस्ति, भाति, प्रिय ही नाम रूप का आधार है। अस्ति अर्थात् अस्तित्व ही भासता है और अस्तित्व ही प्रिय है। अस्ति यानि जो 'है' है, वह सत् है वही भासता है औ इसलिए वह चेतन है। चूँकि वह प्रिय है, इसलिए वह आनंदस्वरूप है। अतः जो 'है है, जो अस्तित्व है वही सत् है, चित् है, आनंद है। उसका न नाम है और न रूप है। वह भास ही भास है, वह अकथ है। जहाँ 'क्या' का विकल्प हुआ कि नाम और रूः पैदा हो गये और माया बीच में आ घुसी। यही नाम रूप माया है, सीता है। यही माया भगवान की उपाधि है जो भगवान को ढाँकती है।
यह माया कब से है? माया तब से है जब से भगवान है, क्योंकि वह पुरुष ई प्रकृति है और भगवान कब से है? जब से माया है, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं ईश्वर है माया है और माया ही ईश्वर है। भगवान कैसे माया हो सकता है? मान्यता ही क नाम माया है। जब भगवान आत्मा को कुछ माना जाता है, तब वही मान्यता माय कहलाती है। इसलिए भगवान ही माया है। कहूँ तो भगवान नहीं और न कहूँ तो माय नहीं, क्योंकि भगवान अकथ है, मन वाणी से परे है। जिसको आत्म ज्ञान हो गया है जिसको स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वही जानता है कि आत्मा अकथ है, अनादि है अनंत है। इसलिए वही आत्मज्ञानी जानता है कि यह नाम रूप वाला जगत् प्रपंच में अपने अधिष्ठान आत्मा के अनुरूप अकथ और अनादि है। कोई नहीं जानता किया प्रपंच कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ व किससे पैदा हुआ। जिसने भी देखा और जर भी देखा, उसे उसी प्रकार उसी रूप में देखा। चूँकि यह प्रपंच भगवान अथवा आत्मा राम पर आधारित है और उससे अभिन्न है, इसलिये यह भी भगवान आत्मा के सदृश अकथ और अनादि है।
माया या प्रकृति भगवान का स्वभाव है। स्वभाव, स्वभावी से भिन्न नहीं होता। जब माया भगवान से अभिन्न है, तब वह भी भगवान के समान अकथ और अनादि है। यद्यपि भगवान अनंत है, अविनाशी है, परन्तु माया अनंत व अविनाशी नहीं है। माया जिस अधिष्ठान आत्मा में कल्पित है, उस सनातन ब्रह्म भगवान राम का बोध या अनुभव हो जाने पर माया का अंत हो जाता है। माया की प्रतीति अज्ञान की हालत में होती है और तब होती है जब उसे उसके अधिष्ठान भगवान आत्मा, राम से भिन्न माना जाता है।
जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, तब माया का भी अंत हो जाता है। यदि उपाधि न हो, तो निरूपाधि भगवान आत्मा को जानने की इच्छा कौन करेगा? नाम रूप उपाधि भगवान आत्मा को छिपाने की झाड़ी है और उस उपाधि के ही कारण सनातन ब्रह्म राम को देखने के लिए जीव को जिज्ञासा होती है। जब स्वरूप का दर्शन हो जाता है तब जीव, ब्रह्म सुख का, आत्मानंद का, अनुभव करता है। जिसने मायापति भगवान आत्मा, राम को जान या पहिचान लिया है, जिसने स्वरूप का अनुभव कर लिया है, उसी ने प्रबला माया को साध लिया है। यह बलवती माया सबसे नहीं सधती। उसे साधने के लिए मायापति भगवान आत्मा राम 'मैं' के स्वरूप का ज्ञान होना अनिवार्य है।
को बड़ छोट कहत अपराधू । सुनि गुन भेद समुझिहहिं साधू ।
देखिअहिं रूप नाम आधीना । रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना ।।
नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहते नहीं बनता। किसी एक को बड़ा कहना या छोटा कहना गलत होगा। साधुजन उनके गुणों का भेद सुनकर उनके बड़प्पन या छुटपन को खुद ही समझ जायेंगे। रूप नाम के अधीन है, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि बिना नाम के रूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता।
भूल से मनुष्य नाम और नामी को दो भिन्न वस्तु मान लेते हैं। कोई नाम को नामी से छोटा और कोई नामी को नाम से छोटा कहते हैं। नाम और नामी में छोटे-बड़े का विचार अनुचित है। नामी अपने नाम से ही जाना जाता है। नाम के बिना नामी की पहिचान नहीं हो सकती। हीरा हाथ में है और उसके मूल्य की कल्पना भी है, परन्तु जब तक उसकी पहिचान नहीं है, हाथ में आया हुआ हीरा भी काँच ही समझा जाता है और मनुष्य उसकी कदर नहीं करता। पहिचान लेने पर, नाम जान लेने पर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। इस तरह नाम की महिमा अपार है। भगवान का नाम भगवान की ही तरह चेतन है और उसकी शक्ति भी असीम है। चूँकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, इसलिए नाम और रूप को एक-दूसरे से छोटा अथवा बड़ा कहना बहुत गलत होगा।
रूप बिसेष नाम बिनु जाने। करतल गत न परहिं पहिचाने ।
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह विसेषे ।।
बिना नाम के जाने हथेली पर रखे हुए पदार्थ की विशेषता अथवा महत्ता नहीं जानी जाती। नाम जान लेने पर यानि पदार्थ की सही पहिचान हो जाने पर वस्तु की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता की सही कीमत आँकी जा सकती है, परन्तु नाम जान लेने पर उस पदार्थ के रूप को देखे बिना भी नामी के लिए हृदय में विशेष प्रेम अथवा आकर्षण पैदा हो जाता है। बिना रूप को प्रत्यक्ष देखे नाम के बार-बार स्मरण से नामी के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न हो जाता है।
नाम रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परति बखानी ।
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥
नाम और रूप अर्थात् माया की गति या महिमा अकथनीय है। यद्यपि समझ जाने पर यह सुख की देने वाली है, परन्तु उस सुख का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वाणी से परे है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान के बीच नाम ही एक सच्चा साक्षी या मध्यस्थ के रूप में है, जो एक चतुर दुभाषिये के समान दोनों का सम्यक प्रकार से ज्ञान अथवा समाधान करता है।
माया की गति या माया की महिमा अपरंपार है, क्योंकि उसका अधिष्ठान भगवान आत्मा की महिमा अनिवर्चनीय है। भगवान की महिमा का ज्ञान हो जाने पर माया की असत्यता का भी बोध हो जाता है और यह भगवान के नाम के स्मरण से सुगम हे जाता है। जिस प्रकार एक चतुर दूभाषिया या दलाल खरीददार और बेचनदार दोनो को मिलाकर दोनों का कार्य करा देता है, उसी तरह नाम रूपी दलाल जापक की भावना के अनुसार सगुण ईश्वर का भी दर्शन कराता है और निर्गुण ब्रह्म का भी बोध कराता है।
मान्यता का ही नाम माया है। कौन मानता है और किसको मानता है? .... यह जान लेने पर वह सुखदायक है, परन्तु उसका निर्णय नहीं किया जा सकता। 'मैं'ने पहले अपने आपको जीव की कल्पना किया। यही कल्पना माया है और यह भगवान के छिपने की झाड़ी है। जब यह मान्यता हट गयी और मायापति का ज्ञान हो गगा, तब जिसका दर्शन होता है वह भगवान आत्मा 'मैं' राम ही है। उस भगवान राम के नाम की महिमा अकथ है और रूप भी अकथनीय है। नाम पहिले लिया जाता है। नाम लेकर पुकारने पर नामी प्रकट होता है और तब उसके रूप का दर्शन होता है। बार-बार नाम लेकर पुकारने से नामी को बरबस आना पड़ता है और पुकारने वाले की ओर ध्यान देना पड़ता है। जिस प्रकार एक अबोध बालक रोकर अपनी माँ को पुकारता है और जब थोड़े रोने पर भी नहीं आती, तब जोर-जोर से और लगातार रो-रोकर पुकारता है और तब माँ को सब काम छोड़कर दौड़कर बच्चे की ओर ध्यान देने के लिए बरबस ही आना पड़ता है, उसी तरह बार-बार नाम जपने से भगवान को अपने जापक भक्त की पुकार पर ध्यान देना ही पड़ता है और दौड़कर आना ही पड़ता है। इसलिए नाम की महिमा अकथनीय है।
अपने इष्ट के नाम का जप चार प्रकार से किया जाता है। मुँह से जो जप किया जाता है उसे बैखरी वाणी कहते हैं। उससे अन्तःकरण शुद्ध होता है और मन का मैल दूर हो जाता है। वैखरी वाणी द्वारा किया गया जप भी दो प्रकार का होता है, एक साधारण और दूसरा प्रांशु। साधारण जप में शब्द जापक के कान में पड़ता है, परन्तु प्रांशु जप में शब्द इतने धीमे से होते हैं कि जापक को भी सुनाई नहीं पड़ते। कंठ से जो जप किया जाता है, उसे मध्यमा वाणी कहते हैं। वह जप स्वप्नावस्था में होता है और उससे विक्षेप दूर होता है। हृदय से जो जप किया जाता है उसे पश्यंती वाणी कहते हैं और वह सुषुप्ति अवस्था में होता है। इससे हृदय पर का आवरण दूर होता है। नाभि से जप होता है उसे परावाणी कहते हैं और वह तुरीयावस्था का द्योतक है। इन सभी जापों में मन से जो मानसिक जप किया जाता है, उसका महत्व अत्यधिक है, क्योंकि उससे जापक का मन निर्विकल्प हो जाता है। इसलिए नाम की महिमा अकथनीय है।
श्री विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, शक्ति, राम, कृष्ण, दत्तात्रेय, गणेश आदि देवताओं में जो भी अपना इष्ट हो और जिनकी उपासना की जाती है, वे सब भगवान की श्रेणी में आते हैं और उनके आगे भगवान की उपाधि लगायी जाती है। जैसे-भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश इत्यादि। अपने इष्ट भगवान की मूर्ति को हृदय देश में अंकित करके उसकी मानसिक पूजा करे। मानसिक पूजा करने के बाद फिर सब अंगों का यानि आठों अंगों का अर्थात् चरण, नाभि, हृदय, कंठ, ग्रीवा, मुख, नासिका भृकुटी का एक के बाद एक ध्यान करें। चरण के ध्यान से शुरू करके भृकुटी में अंत करें। ध्यान इतना गहरा हो कि जिस-जिस अंग का ध्यान किया जाये वह अंग ध्याता के मानस पटल पर निरंतर अंकित हो। जब आखिरी ध्यान भृकुटी में केन्द्रित होता है, तब ध्याता को इष्ट का कोई भी अंग दिखलाई नहीं पड़ता। वह सर्वथा निर्विकल्प हो जाता है, त्रिपुटी का लोप हो जाता है और ध्याता को अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। सबका लोप होने पर देखने वाला स्वयं रह जाता है, इसलिए नाम और रूप की कहानी अकथ है।
प्रबोध तीन प्रकार से होता है, भावना, विचार और जिज्ञासा। हृदय में सगुण मूर्ति की भावना करके इष्ट के नाम का जप किया जाये तो वह नाम का जप सगुण का बोध कराता है। हृदय में विचार करते हुए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा, मेरा क्या अंत होगा आदि पर विचार करते हुए इष्ट के नाम का जप किया जाता है तो वह नाम जप निर्गुण ब्रह्म का बोध कराता है और जब हृदय में ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा लेकर नाम का जप किया जाता है, तब आत्म-तत्व का आत्म स्वरूप का दर्शन होता है। क्योंकि, इष्ट के नाम का जप सगुण और निर्गुण ब्रह्म का यानि जिसकी जो धारणा होती है उसका दर्शन कराता है, इसलिए नाम ही ऐसा सफल दलाल है जो दोनों को यानि जापक और इष्ट को मिला देता है। इसलिए नाम और रूप की महिमा अकथनीय है। किसी संत ने विचार के बारे में कहा है -
को मैं आयों कहाँ ते, कित जैहौं का सार ।।
को मैं जननी को पिता, याको कहत विचार ।।
इस पर गहराई से विचार करने पर ही मनुष्य जन्म सार्थक होता है।
दोहा-
राम नाम मनि दीप घरु, जीह देहरी द्वार ।।
तुलसी भीतर बाहरहुँ, जौं चाहसि उजियार ||21||
तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम इस शरीर रूपी मकान के भीतर और बाहर उजेला (ज्ञान का प्रकाश) चाहते हो, तो जिह्वा रूपी द्वार पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रखो । शरीर एक मंदिर है जिसमें भगवान 'आत्मा' राम स्थापित है। यदि उस भवन के
भीतर और बाहर प्रकाश करना चाहो, तो जीभ रूपी द्वार पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रखो। देहरी पर दीया रखने से भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला होता है। मणि दीपक रखने का भाव यह है कि वह निरंतर प्रकाशित रहता है और पवन के झोकों से (विषय रूपी पवन के झोंके से) बुझता नहीं, जबकि साधन जन्य दीपक हवा के झोकों से बुझ जाता है। राम का नाम मणि दीपक है, जिसे जिह्वा रुपी द्वार पर रखने से भीतर और बाहर, जहाँ दोनों ओर अंधकार रहता है, प्रकाश होता है।
भीतर का अंधकारक्या है और बाहर का अंधकार क्या है? भीतर अंधेरा रहने से यानि हृदय में अज्ञान का अंधकार रहने से जीव अपने आपको जैसा है, वैसा न जानकर, भगवान 'आत्मा' राम न जानकर जीव मानता है और बाहर के अंधकार के कारण अज्ञानियों को भगवान 'आत्मा' राम अपना स्वरूप न भासकर संसार दिखाई देता है।
देहरी के भीतर दीपक रखने से बाहर का अंधकार और द्वार के बाहर दीया रखने से घर के भीतर का अंधेरा दूर नहीं हो सकता, इसलिए राम नाम रूपी मणि दीपक को ऐसी जगह रखना चाहिए (जीभ रूपी देहरी पर) जिससे भीतर और बाहर दोनों तरफ का अंधकार एक साथ समान रूप से दूर हो जाये।
राम नाम रूपी मणि दीपक को जिह्वा रूपी द्वार पर किस प्रकार रखना चाहिए? गले के भीतर कंठ में एक छोटी-सी जीभ है, जिसे कौआ या पडजीभ भी कहते हैं। उस अन्तर्जिह्वा से राम नाम का निरंतर जप करने से साधक तत्काल निर्विकल्पावस्था को प्राप्त हो जाता है और उसका जीव भाव अथवा देह भाव अथवा जगत् भाव अथवा अन्य सभी भावों का अभाव हो जाता है। उसमें केवल 'यावानहम्' - मैं जैसा हूँ-यही भाव रह जाता है। इसतरह अन्तर्जिह्वा से राम नाम का जप करने से जापक जब समाधिस्थ हो जाता है तो उसके समस्त विकल्पों का अभाव हो जाता है। समस्त विकल्पों का अभाव होना ही भीतर और बाहर का प्रकाशित होना है। भीतर ज्ञान के प्रकाश में हृदय में अनादि काल से जो जीव भाव बना हुआ है, उसका नाश होकर आत्म भाव का उदय होता है और शुद्ध सत्य स्वरूप भगवान 'आत्मा' राम का दर्शन होता है। स्व-स्वरूप के दर्शन से अनुभव होता है कि सारा चराचर मेरा स्वरूप है और मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, केवल मात्र अस्तित्व अर्थात् में आत्मा शेष हूँ। बाहर प्रकाश होने पर जिसे हम अज्ञान के अंधकार में जगत् मानते थे, उसका अभाव हो जाता है और सब कुछ राम ही राम भासता है। इस तरह जो राम नाम रूपी मणि दीप को अन्तर्जिव्हा रूपी देहरी (द्वार) पर रखता है, वह सब भावों का (यानि जीव भाव, जगत् भाव व अन्य सब भाव) अभाव करके स्व-स्वरूप भगवान 'आत्मा' रूप का दर्शन करता है और ब्रह्म सुख का अनुभव करता है।
नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी।
ब्रह्म सुखहिं अनुभवहिं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ।।
वे बीतराग योगी ब्रह्म रचित संसार को सर्वथा त्याग चुके होते हैं और जो जीभ से भगवान राम के नाम का जाप करते हैं, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हुए मोह निशा में यानि अविद्या रूपी रात्रि में जागते हैं, उस ब्रह्म सुख या आत्मानन्द का अनुभव ऐसा विकार रहित है, ऐसा अवर्णनीय है कि जिसकी कोई उपमा नहीं, उसका न कोई नाम दिया जा सकता है और न उसका रूप या आकार प्रकार कथन किया जा सकता है।
राम के नाम का वह जप जिससे आत्म सुख का अनुभव होता है, किस प्रकार किया जाता है? कंठ के भीतर जो अन्तर्जिह्वा है, जिसे कौआ या काकल जिह्वा भी कहते हैं, उससे राम का नाम जप करने से मन अविलम्ब निर्विकल्प हो जाता है और उसे संसार के अस्तित्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। उस निर्विकल्पावस्था में वह उस आत्म सुख का अनुभव करता है जो सर्वथा वर्णनातीत है तथा उपमा रहित है। अन्तर्जीभ से नाम जपने से सब प्रपंच का एवं सब भावों का अभाव हो जाता है। जीव भाव तथा जगत् भाव सब खत्म हो जाते हैं। भीतर प्रकाश होने से जीव भाव दूर हो जाता है और बाहर प्रकाश होने से जगत् भाव तिरोहित हो जाता है। भीतर बाहर दोनों ओर प्रकाश होने से जगत् भाव तिरोहित हो जाता है। भीतर बाहर दोनों ओर प्रकाश होने से जापक निर्विकल्पावरथा का, ब्रह्मानंद का अनुभव करता है और यही योगी का अविद्यारूपी रात्रि में जागना है। ऐसे वैराग्यवान योगी की दृष्टि में सिवाय भगवान 'आत्मा' राम के दूसरे का अस्तित्व ही नहीं रहता, उसके लिए नाम रूपात्मक जगत् प्रपंच का सर्वथा अभाव हो जाता है और वही उसका मोह निशा में जागना है। जीव भाव और जगत् भाव, दोनों भावों का अभाव ही वह ब्रह्म सुख है, वह आत्मानन्द है जिसकी कोई उपमा नहीं और जो वाणी के वर्णन से परे है।
राम नाम रूपी मणि दीप को अन्तर्जीभ रूपी देहरी पर रखने से मैं क्या था, मैं क्या हूँ, मैं क्या रहूँगा। मैं क्या था, अब मैं कैसा हूँ और आगे कैसा रहूँगा आदि सब प्रकार के भाव दूर हो जाते हैं और स्वाभाविक निर्विकल्पता आ जाती है। यही अनुपमेव ब्रह्म सुख है, जिसका अनुभव जापक को होता है। साधारण बोलचाल की जीभ से राम नाम का जप करने पर न तो जीव भाव दूर होता है और न जगत् भाव का नाश होता है, ये दोनों भाव बने ही रहते हैं, परन्तु कौआ से जब यह नाम जपा जाता है तब सब भाव लुप्त हो जाते हैं और स्वाभाविक निर्विकल्पता आ जाती है। में ब्रह्म है मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ आदि सब भाव अंधकार के द्योतक है, परन्तु देहरी पर दीपक रखते ही सब भाव तुरंत भाग जाते हैं और आत्म सुख का अनुभव होने लगता है। जिस अवस्था में समस्त भावों का अभाव होता है, वही योगी का मोह निशा में जागना है और वही ब्रह्म सुख है, जिससे किसी प्रकार का सुख व दुःख का अनुभव नहीं होता और जो सर्वथा अनुपमेय है। सुख-दुःख तो मन के विषय हैं, परन्तु ब्रह्म सुख तो इन्द्रियों से परे, मन से परे, स्व-स्वरूप भगवान आत्मा ही है, वहाँ सुख- दुःख को कहाँ स्थान?
आनन्द मुझ आत्मा का एक दृश्य है मैं उसे देखता हूँ, उसे अनुभव करता हूँ। उसी तरह समाधि भी मुझ आत्मा का एक दृश्य है, जिसे मैं जानता हूँ। चित्त की चंचलता में जो दृश्य प्रतीत होता है वह बाहर का दृश्य है और चित्त की एकाग्रता में जो दृश्य प्रतीत होता है वह भीतर का दृश्य है। स्वाभाविक निर्विकल्पता ही योगियों की योग निद्रा है। जिस आनन्द का अनुभव मैं इन्द्रियों के द्वारा करता हूँ, वह वृत्ति जन्य अथवा क्षणिक आनन्द है। उससे इन्द्रियजन्य सुख मिलता है। ब्रह्म सुख अथवा आत्मानंद वह सुख है जो चित्त की स्थिरता और चित्त की चंचलता से सर्वथा असंबंधित है और सदा एक रस रहता है। वह अपना स्वरूप ही है। वाणी उस सुख अथवा आनंद का वर्णन नहीं कर सकती, इसलिए उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। वह अनुपमेय है। वह सुख-दुःख से परे सब विकारों से रहित है। उपमा उस चीज की दी जाती है, जो मन वाणी का विषय है, जहाँ मन वाणी की पहुँच है। जो सुख सापेक्ष (दुःख की अपेक्षा से) होता है, वाणी उसी का कथन करती है, परन्तु जो सुख अपेक्षा रहित होता है, जो सुख-दुःख से परे होता है, जो मन वाणी की पहुँच से बाहर है, वाणी उसे कैसे कथन कर सकती है? इसलिए वह अकथ है।
सामान्य सुख जो हर्ष-विषाद से परे है, वही ब्रह्म सुख है। वह इतना प्रशांत महासागर है कि उसमें न कहीं कोई तरंग है और न कहीं कोई ज्वारभाटा है। विकल्प ही तरंग है और संकल्प ही ज्वारभाटा है। संकल्प-विकल्प रूपी ज्वारभाटा एवं तरंग से रहित ब्रह्मानन्द महान प्रशांत सागर है। वह आत्म सुख इतना मनमोहक प सुंदर है कि कश्मीर भी उसके सामने कुछ नहीं वह इतना शीतल है कि हिमालय भी उसकी अपेक्षा उष्ण है। वह इतना ऊँचा है कि सुमेरु भी उसकी तुलना में नीचा है और वह करोड़ों चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक शांतिदायक है। उस ब्रह्म सुख के अनुभव काल में मुझ आत्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं रहता, केवल 'मैं' ही 'मैं' रहता हूँ। यही आत्म-दर्शन है और यही आत्मानन्द है, जिसकी कोई उपमा नहीं।
सुख अर्थात् सु + ख। सु माने सुन्दर और ख माने आकाशा इसीलिए सुन्दर आकाश ही सुख स्वरूप है। आकाश का जो आकाश वही सुन्दर आकाश है, सुब स्वरूप है, ब्रह्मानन्द है। आकाशवाणी गम्य है, मन गम्य है, बुद्धिगम्य है, कथनीय है, परन्तु जो आकाश का आकाश है, जो ब्रह्म सुख है, वह मन अथवा वाणी अथवा बुद्धि से परे है, इसलिए वह अकथ है। जो ब्रह्म सुख आत्मज्ञानी, बोधवान पुरुष जो अनिर्वचनीय आनन्द का दाता है वहाँ नाम या रूप अथवा माया या संसार किसी की गुंजाइश नहीं। वह सर्व से परे है, इसलिए अकथ है। इसलिए जो ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहे वह राम नाम रूपी मणिदीप को अन्तर्जिह्वा रूपी देहरी (द्वार) पर रखे
जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ । नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ ।
साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाँए ।।
जो भगवान के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे उसके नाम की अभ्यंतर जीन से जप कर जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधकगण में एकाग्रतापूर्वक राम नाम का जाप करके अणिमा, महिमा आदिक सिद्धियों को प्रा कर सिद्ध हो जाते हैं।
जो साधक भगवान के नाम की गूढता को, उनकी यथार्थ महिमा को जानन चाहते हैं अथवा जो ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहते हैं अथवा जो अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वे अन्तर्जिह्वा से राम नाम का जप लय लगाकर करते हैं औ अभीष्ट की प्राप्ति करते हैं। वह नाम, नाम नहीं और वह जप, जप नहीं, जिससे नान का दर्शन न हो, अभीष्ट की प्राप्ति न हो।
जो सुख साधन से प्राप्त होता है वह जीव सुख है, क्षणिक है और जो सुख बिन साधन के मिलता है वह सामान्य सुख है, ब्रह्म सुख है, आत्मानन्द है। अन्तर्जीभ नाम जपना साधन जन्य जप नहीं है, क्योंकि उससे जो ब्रह्म सुख प्राप्त होता है अहंगम्य है, मन वाणी से परे है, इन्द्रियों की पहुँच के बाहर है। वह प्राप्ति की प्राप्ति है जीव सुख या सांसारिक सुख, जो इन्द्रियों के जरिये प्राप्त होता है, वह अप्राप्ति के प्राप्ति है। प्राप्ति की प्राप्ति का सुख यानि ब्रह्म सुख का अनुभव ब्रह्म ही करता है, जो नहीं। जीव भाव के रहते ब्रह्मानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्तर्जिह्वा से नाम जप करने पर मन निर्विकल्प हो जाता है और जीव भाव, जगत् भाव आदि स भावों का अभाव हो जाता है केवल 'मैं' ही 'मैं' का अनुभव होता है और यही ब सुख है। साधारण जीभ से नाम जपने से जीव भाव बना रहता है और सुख-दुखः की प्रतीति होती है। यह जीव सुख है, अभ्यंतर जिह्वा से नाम जपने पर निर्विकल्पता प्राप्त होती है और आत्मानंद का अनुभव होता है। यही नाम की गूढ गति है।
जीव का जीवन भगवान 'मैं' आत्मा है। अभ्यंतर जीभ से नाम जपने पर जीव जीव न रह जाता है, परन्तु साधारण जीभ से नाम जपने पर जीव भाव का अभाव नहीं होता। तब उसे मन की एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है और जब मन एकाग्र होता है, तब जापक को सुख मिलता है। जब मन चंचल होता है, तब जीव जापक को ग्लानि होती है। योगी जब अन्तर्जिह्वा से नाम जपता है, तब उसे मन की स्थिरता अथवा चंचलता की अपेक्षा नहीं रहती। तब मन स्वभावतः निर्विकल्प हो जाता है और सब भावों का अभाव हो जाता है। यही नाम जप की गूढ गति है।
जिसकी गति गूढ़ है, जिसका दर्शन गूढ है, जिसकी महिमा गूढ़ है, जिसका साक्षात्कार गूढ़ है, जिसका जानना गूढ़ है, वह भगवान आत्मा 'मैं' कैसा है, क्या है आदि कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता उस परमात्मा को ऐसा है, वैसा है, कहना सब कपोल-कल्पित है। उस ब्रह्म सुख का जानना इसलिए गूढ़ है कि वह परमात्मा सर्व में, सर्व का सर्व रूप से सब कुछ होकर विद्यमान है। यदि उसमें कुछ विलक्षणता होती तो हर एक का ध्यान उधर जाता, हर एक उसे जानने का प्रयत्न करता। चूँकि 'मैं' आत्मा सर्व में सर्व रूप से सब कुछ होकर रहता हूँ, इसलिए उसकी ओर सर्व साधारण की दृष्टि एकाएक नहीं जाती। इसलिए उस परमात्मा का जानना, उस ब्रह्म सुख का जानना गूढ़ है, उसकी गति गूढ है। जो आँख की आँख है, जो मन का मन है, जो बुद्धि की बुद्धि है, जो वाणी की वाणी है, उसे आँख या मन या बुद्धि या वाणी क्या जाने? इसलिए वह ब्रह्म सुख, वह भगवान आत्मा, वाणी का विषय नहीं है और यही उसकी गूढ़ता है।
लव लगाकर जपना क्या है? साधारण जिह्वा से नाम जपने से जीव भाव बना रहता है और इसलिए मन चंचल रहता है तथा प्रपंच में दौडता है। परन्तु कौआ से नाम का जप करने पर तत्काल लव लग जाती है, क्योंकि तब वृत्तियाँ अन्तर्मुख हो जाती हैं, मन अमन हो जाता है, चित्त चित् हो जाता है और बुद्धि बोध हो जाती है। इस प्रकार नाम जप से साधक अविलम्ब समाधिस्थ हो जाता है और कालांतर में सिद्धियाँ प्राप्त कर सिद्ध हो जाता है।
जपहिं नामु जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी।
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ।।
संसार में भगवान के चार प्रकार के भक्त यानि जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त और ज्ञानी होते हैं और वे चारों ही सुकृति यानि पुण्यात्मा, पापरहित और उदार होते है और नाम जप के अधिकारी होते हैं। आर्त भक्त, जो भारी दुःख से दुखी रहते हैं। भगवान का नाम जप कर अपने कठिन संकट से छुटकारा पाते हैं और सुखी होते हैं। च
हुँ चतुर कहुँ नाम अधारा । ग्यानी प्रभुहि विसेषि पिआरा ॥
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥
इन चारों प्रकार के भक्तों को राम नाम का ही आधार होता है और चारों ही नाम जप के अधिकारी हैं। ध्यान-धारणा में, पूजा-पाठ में, यज्ञ आदि कार्यों में, सबमें भक्तों को भगवान के नाम का ही सहारा है, परन्तु इन चारों प्रकार के भक्तों में प्रभु का ज्ञानी भक्त ही विशेष प्यारा है, भगवान जो चराचर का अस्तित्व है, 'मैं' करके जा सबमें प्रकट है, उसे जो जानता है, उसका जो अनुभव करता है, वह ज्ञानी भत भगवान को विशेष प्रिय है। ज्ञानी भक्त भगवान आत्मा को अपने से भिन्न नहीं मानता वह उसे अभिन्न जानता है। चारों युगों में व चारों वेदों में नाम का महत्व प्रसिद्ध है परन्तु कलियुग में तो उसका विशेष प्रभाव है। नाम जप के सिवाय भवसागर तरने क कोई दूसरा उपाय नहीं है।
दोहा-सकल कामनाहीन जे, रामभगति रस लीन ।
नाम सुप्रेम पियूष हद, तिन्हहुँ किए मन मीन ||24||
जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित हैं और भगवान राम की भक्ति रूपी जर में सर्वदा निमग्न रहते हैं, वे ज्ञानी भक्त भी राम नाम के विशुद्ध प्रेम से भरे हुए अमृत कुण्ड में अपने मन रूपी मछली को सदा डुबाये रहते हैं।
भक्त चार प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के भक्तों में से तीन को अर्थात् आत अर्थार्थी और जिज्ञासु को तो कामनायें (अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष की) रहती हैं परन् ज्ञानी भक्त के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं रहती।
ज्ञानी भक्त सर्वथा निःस्वार्थ और पूर्णरूपेण कामना रहित होते हैं। वे असि भाति, प्रिय रूप से सब में रमने वाले भगवान राम के प्रेम रूपी अमृत कुण्ड में अप मन को मछली बना के डुबाये रहते हैं। जैसे मछली जल में जन्मती है, पलती है, जर में ही खाती है-पीती है, जल में मरती है, उसके आगे जल, पीछे जल, दायें-बार जल, ऊपर-नीचे जल अर्थात् सब तरफ जल ही जल रहता है, वैसे ही ज्ञानी भ अस्ति, भाति, प्रिय वासुदेव से अभिन्न होकर अपने आप में ही आते, आप में ही जाते, आप में ही उठते, आप में ही बैठते, अपने आप में ही सोते, आप में ही जागते, आप में ही खाते और आप में ही पीते हैं। आप ही आगे, आप ही पीछे, आप ही दायें, आप ही बायें, आप ही ऊपर, आप ही नीचे अर्थात् सब ही तरफ अपने आप ही हैं। उनकी दृष्टि में सिवाय भगवान 'आत्मा' राम के कहीं कुछ भी नहीं। वे समस्त व्यवहार करते हुए भी भगवान राम में, अपने स्व-स्वरूप आत्मा में ही वर्तते हैं।
अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ।।
सनातन ब्रह्म भगवान राम, जो अकथनीय, अगाध आदि अन्त रहित व उपमा रहित हैं, उनके दो स्वरूप हैं यानि निर्गुण और सगुण।
भगवान के ये दोनों स्वरूप सगुण और निर्गुण भक्तों की भावनाओं के अनुसार हैं। यथार्थ में वह परमात्मा, वह सर्वात्मा, जो सर्व व्यापक ब्रह्म है, न सगुण है, न निर्गुण है और सब कुछ है। वह पुरुष पुरुषोत्तम सनातन ब्रह्म राम सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है और उससे विलक्षण भी है। आज तक परमात्मा के विषय में संत महात्माओं ने जितना भी विवेचन किया है, सब अनुमान से किया है, परमात्मा उससे भी कहीं ज्यादा विलक्षण है।
भगवान ऐसा है या वैसा है, कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वर्णन करने वाली शक्ति सीमित है और भगवान असीम है, अनन्त है, अपार है, अगाध है। मन वाणी से परे अनिर्वचनीय तत्त्व सीमित उपकरणों द्वारा कैसे बखान किया जा सकता है? शब्दों द्वारा इस अलौकिक विलक्षण व अलख तत्त्व का केवल लक्ष्य कराया जा सकता है।
भाव प्रधान भक्तों को गुणों की दृष्टि से वह परमात्मा सगुण दिखता है और गुण रहित व्यापक दृष्टि वाले ज्ञान प्रधान भक्तों को वही भगवान निर्गुण भासता है। वास्तव में सब दृष्टियों से अतीत तत्त्व एक ही है, अलख है, विलक्षण है। चूँकि आँख उसे देख नहीं सकती, मन वहाँ पहुँच नहीं सकता, बुद्धि उसका निश्चय नहीं कर सकती, चित्त उसका चिंतन नहीं कर सकता इसलिए वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। वह अकथनीय है, अनिवर्चनीय है, क्योंकि किसी ने उसे देखा नहीं, वाणी उसका बखान नहीं कर सकती इसलिए किसी से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, वह अनुपमेय है। वह सनातन ब्रह्म भगवान आत्मा राम अज है, अविनाशी है और आदि अन्त रहित है। कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता कि परमात्मा कब पैदा हुआ और किससे पैदा हुआ? वह सर्वात्मा अनादि है, अनन्त है। वह इतना अपार और असीम है कि कोई उसका पार, अंत व थाह नहीं पा सकता। यदि वह सीमित विभूतियों वाला होता, तब ही कोई उसका पार व थाह पाते अथवा उसका वर्णन कर पाते। तो सब गुणों में ही असीम है और सब दृष्टियों से विलक्षण है। इसीलिए वेदों ने अ नेति-नेति कहकर मौन धारण कर लिया।
भगवान राम सब गुणों से अतीत हैं, जो सब गुणों से अतीत है, उसी में ही गुण रहते हैं। जो किसी एक गुण में आबद्ध हो, उसमें सभी गुण नहीं रह सकते उसमें अनन्त गुण अनादि काल से नित्य निरन्तर रहते हैं, वह वास्तव में सभी गुर से सर्वथा निर्लिप्त है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त आदि शर उस परमात्मा के द्योतक विशेषण हैं न कि उसके वर्णन करने वाले संज्ञा। उसक यथार्थ वर्णन हो ही नहीं सकता, इसीलिए वह अकथनीय है, अनुपमेय है।
यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की यह है कि परमात्मा में एक ही साथ विलक्षण गुणों का समावेश है। परमात्मा जहाँ सगुण है वहाँ निर्गुण भी है। ज साकार है, वहाँ निराकार भी है। जहाँ व्यक्त है, वहाँ अव्यक्त भी है। उसमें ये विरोधी गुण किस प्रकार है, उसे लौकिक दृष्टान्तों द्वारा समझा जा सकता है। काष्टः अग्नि निराकार रूप से व्याप्त होने के कारण प्रगट रूप से दिखती नहीं, पर रू काष्ठ को रगड़ने पर प्रगट हुई अग्नि साकार होकर दिखने लगती है। जल वाष्प रूप में परिवर्तित रहने के कारण निराकार होने से दिखता नहीं, परन्तु वही भाप बादल होकर बरसने लगता है, तब बूँदों के रूप में प्रत्यक्ष दिखता है। जब जड़क व्यक्त और अव्यक्त दोनों हो सकती है, तब चेतन स्वरूप, सर्व शक्तिमान विलक्ष गुणों वाले परमात्मा में यह गुण हों, तो शंका किस बात की?
अतः, जैसे प्रगट अग्नि और गुप्त अग्नि अलग-अलग न होकर एक हैं, प्रल जल और अप्रत्यक्ष जल भिन्न-भिन्न न होकर एक ही हैं, उसी तरह साकार भगव और निराकार ब्रह्म, सगुण ईश्वर और निर्गुण आत्मा दो पृथक शक्ति न होकर एक हैं। ये सब एक ही तत्त्व के, एक ही वस्तु के भिन्न-भिन्न नाम व भिन्न-भिन्न रूप की भावनाओं के अनुसार प्रतीत होते हैं।
मोरे मत बड़ नाम दुहू ते । किए जेहि जुग निजबस निज बूते ॥
मेरी समझ के अनुसार दोनों से अर्थात् सगुण और निर्गुण ब्रह्म से नाम बड अर्थात् अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि नाम के ही बल से, नाम के जप के प्रभाव सगुण ब्रह्म का भी साक्षात्कार याने अनुभव होता है। नाम के ही आधार से सगुण- साकार भगवान का दर्शन तथा निर्गुण व निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है। नाम ऐसा जरिया है, जिससे दोनों प्रकार के ब्रह्म का साक्षात्कार होता है।
प्रौढ़ सुजन जनि जानहिं जन की। कहऊँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ।।
नाम के संबंध में यह जो कुछ भी मैंने कहा है, वह मेरे मन में जैसा विश्वास है, भगवान के प्रति मेरी जैसी प्रीति है और मेरी जैसी रुचि है, उसके अनुसार ही मैंने कहा है। मेरा यह कथन सत्य ही मेरे विश्वास व मेरी प्रीति व रुचि के अनुसार ही है या इसमें कुछ बनावटीपन है, उसे ज्ञानी सज्जनगण, बोधवान भक्तगण, भली-भाँति जानते हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है।
एकु दारुगत देखिअ एकू । पावक जुग सम ब्रह्म बिबेक ।।
अग्नि दो प्रकार की होती है एक गुप्त और दूसरी प्रगट। गुप्त अग्नि अप्रत्यक्ष रूप से लकड़ी में सर्वत्र विद्यमान रहती है और प्रत्यक्ष अग्नि प्रकट रूप से सबको चर्मचक्षु से दिखाई देती है। उसी तरह ब्रह्म भी दो प्रकार है यानि सगुण और निर्गुण अथवा साकार और निराकारा निराकार ब्रह्म गुप्त रूप से सर्वत्र व्यापक है और सगुण ब्रह्म साकार रूप धारण कर संसार में अनेकों चरित्र करता है।
गुप्त अग्नि यद्यपि काष्ठ में सर्वत्र एक समान व्याप्त रहता है तथापि वह किसी को दिखाई नहीं देती और उससे किसी का कुछ काम भी नहीं निकलता। जब वही गुप्त अग्नि लकड़ी को रगड़ने से प्रगट की जाती है तब वह सबको दिखाई देती है और उससे संसार का बहुत-सा काम भी होता है। उसी तरह ब्रह्म को समझना चाहिए। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म चराचर में सर्वत्र एक समान व्याप्त है, परन्तु जो किसी को दिखाई नहीं देता वही नाम जप के रगड से भक्तों के द्वारा प्रगट किया जाता है और तब व संसार वालों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। वही साकार रूप धारण करने वाला भगवान भक्तों के कल्याणार्थ व देवता, ब्राह्मणों के रक्षणार्थ तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए अनेको सुन्दर चरित्र करता है। सगुण परमात्मा का प्रादुर्भाव संसार में इसी निमित्त होता है।
उभय अगम जुग सुगम नाम ते। कहउँ नामु बड़ ब्रह्म राम ते ।।
दोनों (सगुण और निर्गुण) अगम हैं, परन्तु नाम जप से दोनों सुगम हो जाते हैं और इसलिए मैं निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम को बड़ा कहता हूँ। निर्गुण ब्रह्म अगम है इसलिए कि वह चर्मचक्षु से किसी को दिखाई नहीं देता और
उसके जप में कोई आधार नहीं होता। निर्गुण ब्रह्म का जप निरालंब होता है इसलिए वह अगम है। सगुण ब्रह्म चूँकि आकार-प्रकार वाला होता है इसलिए वह सबों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। सगुण ब्रह्म संसार में साधारण मनुष्यों के समान अनेकों चरित्र करता है जिन्हें देखकर बड़े-बडे ज्ञानी पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं।
इसलिए सगुण भगवान भी अगम है अर्थात् उसकी गति समझ में नहीं आती भगवान के नाम के जप से दोनों प्रकारके ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है इसलिए ब्रह्म सगुण तथा निर्गुण की अपेक्षा नाम ज्यादा बड़ा है अर्थात् अधिक प्रभावशाली है।
ब्यापकु एक ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन घन आनंद रासी ॥
अस प्रभु हृदयें अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ नाम निरूपन नाम जतन ते। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥
वह ब्रह्म जो एक है, अज है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, सत्य स्वरूप है चैतन्य घनभूत है और आनंद का सागर है, ऐसे सर्वथा विकार रहित भगवान के हृदय में विराजमान होते हुए भी संसार के सारे जीव दीन व दुःखी हैं (यह बड़े अचम्भे की बात है) परन्तु नाम के यत्न से यानि नाम के जप से राम का महत्व उसी प्रकार प्रगट हो जाता है, जिस तरह रत्न के परख हो जाने पर उसकी कीमत की जानकारी ह जाती है।
ईश्वर एक है। हर मजहब वाले ईश्वर को एक मानते हैं। यदि ईश्वर एकः अधिक होते तो हर एक ईश्वर के बनाये हुए मनुष्य अलग-अलग प्रकार के होत मुसलमानों के (ईश्वर) खुदा के बनाये हुए मनुष्य हिन्दुओं के भगवान राम या कृष के बनाये हुए मनुष्यों से भिन्न होते या ईसाइयों के ईश्वर ईसा के बनाये प्राणी मूसा बनाये हुए प्राणियों से भिन्न किस्म के होते या राम के बनाये हुए मनुष्य शैवों के ईश्व शिव के बनाये हुए आदमियों से अलग ही प्रकार के होते। परन्तु, ऐसा है नहीं। सब मनुष्य, सब धर्म अथवा मजहब के मानने वाले मनुष्य एक ही प्रकार के होते यद्यपि हर मजहब वालों के ईश्वर के नाम भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु वे सब नाम एक तत्त्व के हैं, एक ही शक्ति या अस्तित्व के हैं। इससे सिद्ध है कि ईश्वर एक है जो सबर आधार है, सबका आत्मा है। उस एक के बिना किसी की सिद्धि नहीं, क्योंकि भगवा एक है और सबका आधारभूत है, उसका किसी से भेद नहीं। वह सबसे अभेद रूप और सबमें अभेद रूप से व्याप्त है। ब्रह्मा से लेकर एक कण पर्यन्त वह सारे चर-अ में एक-सा व्याप्त है। इस तरह वह सर्वाधार आत्मा राम जो एक है, सर्वव्यापक भी
जो सर्वव्यापक होता है, जो सर्व में अभेद रूप में व्याप्त रहता है, वह आकार प्रकार से रहित होता है। वह निरवयव निराकार होता है, उसका न आदि होता है न अंत, उसका कभी नाश नहीं होता। नाश होता है आकार-प्रकार का। जिसका कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, वह कैसे नाश होगा। वह अविनाशी होता है। भगवान आत्मा 'मैं' का कोई आकार-प्रकार नहीं, वह निराकार है इसलिए अविनाशी है।
भगवान आत्मा राम यानि 'मैं' का धर्म जानना है। 'मैं' आत्मा कद से जान रहा हूँ कोई नहीं जानता। 'मैं' आदिकाल से जानते आ रहा हूँ और अनंत काल तक जानता रहूँगा। 'मैं' बिना किसी उपकरण के जानता हूँ। मेरा जानना धर्म अविनाशी है। चूँकि, धर्म धर्मी से भिन्न नहीं होता, इसलिए मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अखण्ड हूँ। परात्पर भाव में आत्मा, भगवान राम का ज्ञान अखण्ड है। 'मैं' आत्मा जानते - जानते कभी नहीं थकता और सबको जानता हूँ। 'मैं' आत्मा जागृत अवस्था के प्रपंच को जानता हूँ, स्वप्न के प्रपंच को जानता हूँ और सुषुप्ति के आनंद को भी जानता हूँ। 'मैं हूँ' का ज्ञान सबको है। यद्यपि सुषुप्ति अवस्था में मैं' और हूँ का ज्ञान नहीं रखता फिर भी 'मैं' आत्मा का परात्पर भाव सर्वदा सब काल में और सर्व अवस्था में रहता है। परात्पर भाव कालातीत है, अवस्थातीत है, भावातीत है, नित्य है इसलिए अविनाशी है।
फिर, वह परमात्मा ब्रह्म है। ब्रह्म वह है जो ब्रह्मा से आदि लेकर कण पर्यन्त सारे चराचर को आच्छादित कर रखा है और जिससे बाहर निकल कर कोई जा नहीं सकता। ब्रह्म के माने वृहत् भी होता है अर्थात् जो बडे से भी बड़ा है। चूँकि भगवान राम एक है, अस्तित्व रूप है, उससे न कोई बडा है और न कोई छोटा है। वह ब्रह्म है, वह महात्मा है।
फिर भगवान राम सत् है, चित् है, आनंद का भण्डार है। भगवान का नाम र + आ+ म का संयोग है। रकार चित्वाचक है, आकार सत्वाचक है और मकार आनंदवाचक है। यानि भगवान राम सत् + चित् + आनंद का द्योतक है। सत् वह है, जिसका कभी नाश नहीं होता और जो सर्वकाल एक-सा विद्यमान रहता है। भगवान राम सत्य स्वरूप है, अविनाशी है। चित् अर्थात् चेतन अर्थात् चैतन्य गुण वाला वह है जो चेतन स्वरूप है, जो भूत वर्तमान व भविष्य सबको जानता है, सब कुछ जानता है और जिसके लिए अज्ञात कुछ भी नहीं। वह ज्ञानस्वरूप ही है। आनंद वह है, जो सबको प्रिय है, जिसको सब चाहते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए सभी सर्वकाल प्रयत्न करते हैं। भगवान राम ज्ञान स्वरूप होते हुए आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप है, क्योंकि उसको पाने के बाद किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रहती। उस भगवान राम को प्राप्त करजीव सब कुछ भूल जाता है, सब प्रयत्नों का अंत हो जाता है, क्योंकि वह तो आनंद का भण्डार ही है, आनंद स्वरूप ही है। इस तरह भगवान 'आत्मा' राम जो अज है, अविनाशी है, एक है, ब्रह्म है, व्यापक है, वह सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप भी है, इसलिए श्रुति ने उस सनातन ब्रह्म के लिए सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् कहा है।
सर्व व्यापक होने के नाते भगवान राम घट-घट के वासी हैं, सबके हृदय में। निवास करते हैं। अब यहाँ शंका होती है कि आनंद के सागर भगवान राम जब सबके हृदय में निवास करते हैं। तब संसार के समस्त जीव दीन व दुःखी क्यों रहते हैं? जब आनंद स्वरूप भगवान हृदय में निवास करते हैं, तब जीव को दुःखी नहीं होना चाहिए। जीव का दीन व दुःखी होने का कारण है, उसका अपने स्वरूप का भूलना। जीव यथार्थ में ब्रह्म है, सत् चित् आनंद है, अज है, अविनाशी है। जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। परन्तु, जीव अपने को ब्रह्म से भिन्न क्षुद्र, अल्प शक्ति वाला, निर्बल, एक देशीय, परिछिन्न, असत्, जड़, जन्मने मरने वाला, विकारवान, सुखी- दुखी, पापी-पुण्यी आदि मानता है। उसकी धारणा है कि वह माया के वश में है और माया के वश में होने के कारण वह दीन व दुःखी है तथा जन्मता, मरता है। इसी हीन मान्यता के कारण ही वे सब प्राणी जो अपने को क्षुद्र संसारी जीव मानते हैं, दीनव दुःखी रहते हैं। यदि उनकी जीव भावना का अंत हो जाये, यदि वे यथार्थ में अपने को ब्रह्म या आत्मा या राम जानें, यदि उन्हें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाये, तो उनके सारे दुःख दूर हो जायें और वे ब्रह्मानन्द का सुख उसी प्रकार अनुभव करें जिस प्रकार जौहरी या पारखी के द्वारा रत्न की परख एवं मोल हो जाने पर दरिद्र मनुष्य सुर्ख होते हैं।
रत्न यद्यपि बहुत मूल्यवान होता है तो भी वह एक अनाडी कुंजड़े के हाथ कंकड़ पत्थर के समान है। जब किसी पारखी के द्वारा उस रत्न की परख हो जाती है और जब वह शान पर चढकर सुन्दर आकार व अपने स्वाभाविक चमक को प्राप्त कर लेता है, तब उसके वास्तविक मूल्य की जानकारी होती है, जिस प्रकार रत्न के यथार्थ मूल्य की जानकारी हो जाने पर रत्न का स्वामी सुखी होता है, उसी तरह नाम जप से स्व-स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जीव को आत्मानंद की प्राप्ति होती है और उसके सारे दुःख दूर हो जाते हैं। आत्मानंद की प्राप्ति अर्थात् स्व-स्वरूप का ज्ञान नाम के जप से अन्तर्जिह्वा से नाम का जप कर जीव को होता है। इस तरह नामक जप ही सब सुखों का भण्डार है। यहाँ पर ब्रह्म या स्व-स्वरूप की उपमा रत्न से हैं गयी है और ब्रह्म का ज्ञान मूल्य को आँकता है तथा रत्न का परखना है।
दोहा-निर्गुन ते यहि भाँति बड़, नाम प्रभाउ अपार ।
कहउँ नामु बड़ राम तें, निज बिचार अनुसार ।।24।।
इस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म से नाम बड़ा है तथा नाम का प्रभाव भी असीम है। अब अपने विचार के अनुसार भगवान राम से भी नाम को बडा तथा अधिक प्रभावशाली कहता हूँ।
राम भगत हित नर तनु घारी। सहि संकट किए साधु सुखारी ॥
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगल बासा ।।
श्री रघुनाथ जी ने भक्तों के कल्याण करने के निमित्त मनुष्य शरीर धारण किया और स्वतः अनेकों दुःख सहकर साधु जनों को सुख पहुँचाया। परन्तु, जो भक्त प्रेमपूर्वक उनके नाम का जप करते हैं, वे सहज ही आनंद व कल्याण के घर हो जाते हैं।
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ।।
रिषि हित राम सुकेतु सुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ।।
सहित दोष दुख दास दुरासा । दलइ नामु जिमि रबि निसि नासा ।।
श्री रामचन्द्र जी ने एक ही ऋषि पत्नी का अर्थात् गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का उद्धार किया। श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी व अन्य ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के निमित्त सुकेतु की पुत्री ताड़का का उसकी सेना व दोनों पुत्र सुबाहु एवं मारीच सहित नाश किया। परन्तु, उनका नाम भक्तों की गयी हुई आशाओं को फिर से जगाकर पूर्ण कर देता है तथा उनके दोष और दुःख को इस प्रकार सम्पूर्ण नष्ट कर देता है जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार का नाश करता है।
भंजेउ राम आप भव चापू । भव भय भंजन नाम प्रतापू ।।
दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन। जन मन अमित नाम किए पावन ।।
निसिचर निकर दले रघुनंदन। नामु सकल कलि कलुष निकंदन ।।
श्री रामचन्द्र जी ने स्वतः तो भगवान शंकर के धनुष को ही तोडा, परन्तु उनके नाम की ऐसी महिमा है कि उसका जप करने वालो को संसार चक्र में फँसने का भय ही दूर हो जाता है अर्थात् वे जन्म-मरण के दुःख से तथा आवागमन के चक्र को तोड़कर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। भगवान राम ने तो अकेले दंडकवन को शाप मुक्त करके उसे रमणीय व पवित्र बनाया, परन्तु उनके नाम ने असंख्य भक्तों के मन रूपी वन को सुन्दर व पवित्र बना दिया। रघुनाथ जी ने तो केवल राक्षसों के समूह का नाश किया, परन्तु उनके नाम के स्मरण से कलियुग के समस्त पापों का नाश होता है।
दोहा-सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ ।
नाम उघारे अमित खल बेद बिदित गुननाथ ||25||
रघुनाथ जी तो भीलनी शबरी, गिद्ध जटायु और कुछ सद्भक्तों को सद्गकि दिया, परन्तु नाम ने तो असंख्य पापियों का उद्धार किया, जिनकी गाथा वेदों वर्णित है।
राम सुकंठ बिभीषन दोऊ । राखे सरन जान सबु कोऊ ॥
नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद बर बिरिद बिराजे ॥
श्री रामचन्द्र ने सुग्रीव और विभीषण इन दोनों शरणागतों की रक्षा की यह बान सब कोई जानते हैं, परन्तु नाम ने तो अनेकों दीन दुःखी शरणागतों का उद्धार किया जिनकी कथा संसार में वेदों में प्रगट है।
राम भालु कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा ॥
नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु बिचारु सुजन मन माहीं ॥
श्री रघुनाथ जी ने रीछ व बन्दरों की बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर समुद्र के एक छोटे से हिस्से पर पुल बाँधने के लिए बहुत परिश्रम किया, परन्तु उनके नाम के स्मरण से ही सारा संसार-सागर सूख जाता है। हे सज्जनगण! आप लोग अपने मन में इस पर विचार करें।
रामेश्वर से लंकापुरी पहुँचने के लिए श्रीरामचन्द्र जी ने 400 कोस चौडा समुद्र के टुकड़े पर पुल बाँधने के लिए करोड़ों भालू व वानरों की सहायता ली, परन्तु राम के नाम के स्मरण से सारा भव सागर ही सूख जाता है। अब यहाँ पर विचार करना है कि वह राम कौन है, जिसका नाम लेने से भव सागर सुख जाता है और उसका नाम किस प्रकार लिया जाये? 'रमुक' क्रीड़ायाँ धातु से 'राम' शब्द बनता है। जो सारे चराचर में ब्रह्मा से आदि लेकर कण पर्यन्त सब में रम रहा है, जिसमें योगी महाल जन रमण करते हैं, उसे कहते हैं राम। जिसे आँख देख नहीं सकती, कान सुन नह सकता, त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती, वाणी बखान नहीं कर सकती, मन जहाँ पहुँच नहीं सकता, बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती, चित्त चिंतन नहीं कर सकता, वह इन्द्रियों से परे, गुणों से अतीत, सर्व व्यापक भगवान राम हैं। वह वही राम है, जो रूप सर्व का आत्मा है, सर्व का सर्व है, सारे चराचर का आधार है और सब में अस्तिद रूप से रम रहा है। ब्रह्मा से आदि लेकर कण पर्यन्त कोई भी देश, कोई भी वस्तु कोई भी अवस्था तथा कोई भी काल ऐसा नहीं जो उस राम से, जो उस अस्तित्व से रहित हो वही अस्तित्व 'है' ही राम है, जो सब में 'व' करके प्रसिद्ध है, प्रगट है। 'है' और 'मैं' ये दोनों ही अनुभव करने योग्य या साक्षात्कार करने योग्य है। वही वह राम है, जिसके स्मरण से भव सागर सूख जाता है।
भगवान आत्मा राम जो सर्व का आधार है इस जगत् प्रपंच का भी जो जड़ है, मिथ्या है, स्वप्नवत् है, माया रचित है, आधार है। भगवान पर आधारित होने के कारण यह जगत् प्रपंच भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है, क्योंकि अध्यस्थ अधिष्ठान के ही अनुरूप होता है। जो प्राणी अज्ञानवश उसे भगवान से भिन्न मानता है, उसके लिए यह संसार आवागमन का कारण होता है, परन्तु जो उसे अधिष्ठान भगवान आत्मा का स्वरूप जानता है, उसके लिए संसार का अत्यन्ताभाव हो जाता है, उसकी दृष्टि में संसार नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह जाती, उसके लिए भवसागर सूख जाता है, जो अधिष्ठान भगवान 'आत्मा' राम को 'है' या 'मैं' को अपना स्वरूप जानता है, जिसकी उसमें अटूट निष्ठा है, जिसकी दृष्टि में भगवान आत्मा 'मैं' के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, उसके लिए भवसागर सूख जाता है, उसके लिए भवसागर का सर्वथा अभाव ही हो जाता है। सर्व दृश्यमान को भगवान आत्मा राम का स्वरूप जानना, अपने आपके अतिरिक्त कहीं कुछ न देखना, सर्वदा अपने स्व-स्वरूप में स्थित रहना ही भगवान राम का स्मरण है, भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है।
जीव अपने को शरीर मानकर अभिमान करता है कि यह देह में हूँ और यह देह मेरा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। शरीर जन्म लेता है, बढता है, क्षीण होता है, वृद्ध होता है और अंत में नाश हो जाता है। परन्तु, आत्मा सभी अवस्थाओं में जैसे का तैसा रहता है, एक स्वरूप रहता है, वह न तो जन्मता है और न मरता है। उस आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न अस्त्र- शस्त्र छेदन कर सकते हैं या काट सकते हैं। वह सदा सर्वदा शांत, निर्विकार, निश्चय, एक रस रहता है, वह सब कुछ देखता है, सुनता है तथा अनुभव करता है। वह आत्मा हम स्वयं हैं, शरीर से सर्वथा भिन्न।
जब तक देहाध्यास है, तब तक देहाभिमान है और जब तक देहाभिमान है, तब तक जीव आवागमन के चक्र में फँसे रहकर जन्म-मरण का दुःख भोगते रहता है। आवागमन का चक्र तभी टूटता है जब जीव भाव का अभाव होकर आत्म भाव का उदय होता है। जब तक व्यक्ति जीते जी नहीं मर जाता भव सागर नहीं सूखता। जब तक व्यक्ति अपने आपको शरीर मानता है, तब तक जीता है। जब देह भाव त्याग कर आत्म भाव लाता है, जब अपने आपको भगवान आत्मा 'मैं' जानता है, तब वही उसका जीते जी मरना है। अपने आत्म स्वरूप को पहिचानकर अपने 'मैं' को भगवान आत्मा 'मैं' जान लेने पर व्यक्ति जीते जी मरता है। जिसकी दृष्टि में भगवान आत्मा 'मैं' के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, उसी के लिए भव सागर सूखता है। जिस प्रकार प्रकाश या सूर्य देश में अंधकार कहीं दिखाई नहीं देता, अंधकार देश में ही अंधकार दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्म देश में देखने पर प्रपंच कहीं दिखाई नहीं देता। प्रपंच तो मान्यता देश की यानि जीव देश की वस्तु है। अतः, जिसे आत्म स्वरूप का ज्ञान है, जिसकी अपने स्वरूप आत्मा 'मैं' में दृढ़ निष्ठा है, ईश्वर में अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है उसी के लिए भव सागर सूखता है और वही भवसागर तरता है। इस प्रकार विचार कर जो सज्जन अपने स्व-स्वरूप में निमग्न रहते हैं, वे अनायास ही भवसागर पार हो जाते हैं।
राम सकुल रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥
राजा रामु अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बर बानी ।।
श्री रामचन्द्र जी ने युद्ध में रावण को उसके समस्त कुल सहित मारा और सीता जी के साथ अपने नगर अयोध्या को लौट आये। फिर राजगद्दी ग्रहण कर अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर राज्य किये, जिसका गुण गान सुन्दर वाणी से देवता व मुनि वृन्द करते हैं।
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती । बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती ॥
फिरत सनेहैं मगन सुख अपने । नाम प्रसाद शोच नहिं सपने ॥
जो सेवक, जो भक्त प्रेमपूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करते हैं यानि आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, वे अनायास ही मोह या माया को उसके पूरे दल सहित जीत लेते हैं और निजानन्द की मस्ती में मस्त आनन्दपूर्वक विचरते हैं। नाम के प्रभाव से स्वप्न में भी उन्हें किसी प्रकार का सोच व दुःख नहीं होता।
यहाँ पर मोह या अज्ञान से रावण और मोह दल से कुंभकर्ण, मेघनाथ व अन्य प्रबल राक्षसों की ओर संकेत है। आठ चक्रों व नव द्वारों की अयोध्यापुरी जैसी यह मानव देह है, जिसमें भगवान आत्मा 'मैं' का निवास है और अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठना मानो आत्मानन्द में स्थित होना है।
राम को रावण व उसके बलवान सैन्य दल को नाश करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, परन्तु राम के भक्तगण राम नाम का प्रेमपूर्वक स्मरण करके सुगमता पूर्वक मोह या अज्ञान तथा अज्ञान जनित काम, क्रोध, लोभ आदि मोह के प्रबल सैन्य दल को नष्ट कर देते हैं। जो बोधवान पुरुष अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते है, उनकी दृष्टि में न तो प्रपंच रहता है, न विषय रहते हैं और न विषयों को ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ रहती हैं। उनकी दृष्टि में विषयों का तथा विषयों को विषय करने वाली इन्द्रियों का सर्वथा अभाव रहता है। वहाँ शुद्ध आत्मा 'मैं' के अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं। अतः, काम, क्रोध, लोभ आदि अज्ञान जनित सर्व विकार, इन्द्रियाँ अथवा माया जनित समस्त विकार आप ही नष्ट हो जाते हैं और आत्मनिष्ठ पुरुष अपने स्वरूपानन्द में मस्त शोच व शोक रहित विचरते हैं।
दोहा-ब्रह्म राम तें नामु बड़ बर दायक बर दानि ।
राम चरित सत कोटि महँ लिय महेस जियें जानि ॥26॥
इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण रूपधारी भगवान राम दोनों से भी बड़ा एवं अधिक प्रभावशाली है और ब्रह्मा जैसे बड़े-बड़े वरदाताओं को भी वर देने वाला है। ऐसा हृदय में विचार कर करोडों रामचरित्र में से महादेव जी ने राम नाम के दो अक्षरों को सार जानकर धारण कर लिया।
नाम प्रसाद सँभु अबिनासी । साजु अमंगल मंगल रासी ।।
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी ।।
नाम के प्रभाव से शंकरजी अविनाशी हो गये और उनके शरीर पर का अशुभ वेष व साज-सज्जा (मुंडमाला तथा श्मशान की भभूति) मंगलकारी हो गया। नाम के ही प्रताप से शुकदेवजी, सनक सनन्दन बन्धु, सिद्धगण, मुनिवृन्द, योगी जन आदि सब ब्रह्मानन्द का सुख भोगते हैं।
नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ।
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ।।4।।
नाम की महिमा को नारद जी ने जाना और इसलिए उस नाम के जप के प्रभाव से वे उन भगवान राम और शिवजी को प्रिय हैं, जो सारे संसार को प्रिय हैं व पूज्य है। भगवान के नाम के जप के ही प्रताप से प्रह्लाद जी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सके और भक्तों के सिरताज बन गये।
ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ । पायउ अचल अनूपम ठाऊँ ।
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू ।।
अपनी सौतेली माँ के कटु वचनों से दुःखी होकर ग्लानि के कारण ध्रुवजी ने दुःख के हरने वाले भगवान हरि के नाम का जप किया और फलस्वरूप अचल और उपमा रहित स्थान प्राप्त किया। अंजनिपुत्र हनुमान ने भगवान राम के पवित्र नाम का जप कर भगवान को ही अपने वश में कर लिया अर्थात् भगवान राम के अतीव कृपा-पात्र हो गये।
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ । भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥
कहाँ कहाँ लगि नाम बड़ाई । रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥
इनके अतिरिक्त पापी अजामिल, ग्राह पीड़ित गजेन्द्र इन्द्रद्युम्न, वेश्या पिंगला आदि सब नाम के जप के प्रताप से पापों से अथवा संकट से मुक्त हो गये। नामों की बड़ाई अथवा महिमा मैं कहाँ तक गाऊँ। नाम की महिमा का बखान मैं नहीं कर सकता। स्वतः भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते।
नामी से नाम भिन्न नहीं जो गुण नामी में है, वे सभी गुण नाम में भी हैं। भगवान राम अनन्त हैं, अपार हैं, असीम हैं, इसलिए उनके नाम भी अनन्त हैं, अपार हैं, असीम हैं तथा उनके गुण भी अनन्त हैं, अपार हैं, असीम हैं, चूँकि भगवान राम के गुणों का वर्णन मन, वाणी से परे है, इसलिए उनके नाम के गुणों का वर्णन भी मन वाणी का विषय नहीं है। किसी भी वस्तु का बखान वाणी के द्वारा किया जाता है। जब भगवान राम के नाम के गुणों का वर्णन मन, वाणी से परे है, तब स्वतः भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन किस प्रकार कर सकेंगे, क्योंकि नाम की महिमा का बखान भी वे वाणी के द्वारा ही करेंगे। अतः, भगवान राम भी अपने नामों की महिमा का कथन करने में असमर्थ होंगे।
नाम बीज है। बीज के अंदर विशाल वृक्ष सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप में छिपा हुआ रहता है। वह पहिले तो दिखाई नहीं देता, परन्तु बाद में अंकुरित होने पर एवं बढने पर स्पष्ट दीख पड़ता है। जैसे बीज के अंदर जड़ पिंड, शाखायें, पत्ते, फूल, फल इत्यादि सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं, वैसे ही नाम में भगवान के सभी गुण समाविष्ट रहते हैं। जब नाम का जापक श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम का जप करता है, तब उसे वे सभी फल मिलते हैं, जिसकी आकांक्षा वह भगवान से करता है। नाम का प्रभाव बडा भारी है। यदि नाम को नामी से बढ़कर कहा जाये तो कुछ अत्युक्ति नहीं होगी इसलिए नाम की महिमा का गायन स्वतः भगवान राम भी नहीं कर सकते।
दोहा-नामु राम को कल्पतरु, कलि कल्यान निवासु ।
जो सुमिरत भयो भाँग ते, तुलसी तुलसीदासु 126।।
तुलसीदास जी कहते हैं कि कलियुग में भगवान राम के नाम का स्मरण स्वर्ग की विभूति कल्पवृक्ष के समान सर्वकामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा सब प्रकार के कल्याण का दाता है। वे कहते हैं कि उस नाम के जप से में स्वत जो भांग के समान त्याज्य था, तुलसी के समान भगवान को प्रिय व ग्राह्य हो गया। तात्पर्य, भगवान राम के भजन के प्रताप से विषयी तुलसीदास भगवान के भक्त व कृपापात्र हो गये।
चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। भए नाम जपि जीव बिसोका ।।
बेद पुरान संत मत एहू - सकल सुकृत फल राम सनेहू ।।
चारों युग में, तीनों लोक में और तीनों काल में (भूत, वर्तमान, भविष्य) भगवान के नाम को जप कर जीव शोक रहित हो गये अर्थात् सुखी हुए। वेदों का, पुराणों का व संत महात्माओं का सब का यही मत है कि भगवान राम के नाम में प्रेम होना सब पुण्यों का फल है। पूर्वार्जित पुण्यों के उदय होने पर ही भगवान राम के प्रति सहज स्नेह होता है, जो कैवल्य पद का देने वाला है।
ध्यानु प्रथम जुग मख बिधि दूजे । द्वापर परितोषत प्रभु पूजे ।।
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ।।
प्रथम युग सतयुग में ध्यान धारणा से, द्वितीय युग त्रेता में यज्ञादि से और तृतीय युग द्वापर में पूजा-पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं। चौथा युग कलियुग केवल पाप की जड व खानि है और उस गंदे पाप के समुद्र में लोगों की मन रूपी मछली रात-दिन डूबी रहती है।
नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला ।।
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥
भगवान राम का नाम भयंकर काल के समान है और स्मरण करने से भवसागर के सारे जल को यानि जन्म मरण के फन्दे को नष्ट कर देता है। फिर कलियुग में भगवान राम का नाम कल्पवृक्ष के समान सब कामनाओं को पूरा करता है तथा इस मृत्यु लोक में माता-पिता के समान एवं परलोक में मित्र के समान हित का साधने वाला है। तात्पर्य यह है कि भगवान राम के नाम के जप से इस लोक में सुख तथा मृत्यु उपरान्त सद्गति की प्राप्ति होती है। नाम के स्मरण से संसार का आवागमन का चक्र नष्ट होता है।
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू । राम नाम अवलंबन एकू ।।
कालनेमि कलि कपट निघानू। नाम सुमति समरथ हनुमानू ।।
कलियुग में न तो निष्काम कर्म ही होता है, न तो ज्ञानोपार्जन हो सकता है और न भक्ति ही की जा सकती है। उसमें केवल मात्र एक राम नाम का सहारा है। कलियुग कालनेमी राक्षस के समान पाप व कपट का भण्डार है और भगवान का नाम उसके नाश करने के लिए बुद्धिमान हनुमान के समान समर्थ है। भाव यह है कि जिस प्रकार चतुर हनुमान जी ने काल-नेमि राक्षस के कपट को भेद कर उसका नाश किया, वैसे ही भगवान राम का नाम कलियुग के पापों का अंत कर देता है।
दोहा-राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल ।
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥27॥
भगवान राम का नाम नरसिंह के समान है, कलियुग दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सदृश है और राम नाम के जपने वाले भगतगण प्रहलाद के जैसे हैं। जिस प्रकार देवताओं के बैरी हिरण्यकश्यप को मार कर नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार राम नाम रूपी नरसिंह भगवान कलियुग रूपी हिरण्यकश्यप का नाश कर नाम जपने वाले प्रहलाद रूपी भक्तों की रक्षा करते हैं।
तात्पर्य यह है कि कलियुग में राम नाम का जप कलियुग के सम्पूर्ण पापों को नाश कर जापक को इस लोक में सुख देता है तथा उनके परलोक को सुधारता है। उनको सद्गति देता है और वे निजानन्द की मस्ती में मस्त रहकर विचरते हैं। राम का नाम चाहे जिस भाव से भी जपा जाय, वह सब प्रकार से कल्याणप्रद ही होता है। इसीलिए कहा भी है कि "भायें कुभायें अनखे आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।"
भायँ कुभायँ अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करउँ नाइ रघुनाथहि माथा ।।
भगवान राम का नाम अच्छे भाव से भजो, चाहे बुरे भाव से भजो, ईर्ष्या से भज चाहे आलस्य से भजो, भजने से सब ही दिशाओं में सब प्रकार का कल्याण होग उस कल्याणकारी राम के नाम का स्मरण कर तथा उन रघुनाथजी के चरणो प्रणाम कर उसके गुणों की गाथा की रचना करूँगा।
भगवान के नाम का जप चाहे जिस भाव से भी किया जाये, वह सर्वकाल व सर्व अवस्थाओं में सर्वत्र कल्याणकारक होता है। वह जप यदा-कदा न होकर निरंतर होवे, तब ही वह उत्तम है। प्रेम भाव से या सद्भाव से भजने वाले तो संसार सागर से तर ही जाते हैं, परन्तु ईर्ष्या भाव से या बैर भाव से या आलस्य से भजने वालों को भी वे दयानिधान प्रभु परमपद देते हैं। दशरथ, कौशल्या तथा वसुदेव, देवकी ने भगवान को वात्सल्य भाव से भजा, गोपियों ने पतिभाव से भजा, अर्जुन व उद्धव ने सखा भाव से भजा, विभीषण ने सद्भाव यानि भक्ति भाव से भजा, हनुमान व भरत ने सेवक भाव से भजा, कुम्भकरण ने आलस्य भाव से भजा, बालि ने अनख अर्थात् ईर्ष्या भाव से भजा और रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, शिशुपाल आदि ने कुभाव यानि बैर भाव से भजा। दशरथ से लेकर हनुमान व भरत तक के सब भक्तों को सद्गति तो मिली ही, परन्तु कुम्भकरण, बालि, रावण, कंस आदि को भी, जिन्होंने भगवान को आलस्य तथा अनख से भजा, करुणासागर प्रभु ने मोक्ष पद दिया। बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान के निरंतर स्मरण के किसी की सद्गति नहीं होती।
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती ।।
वे कृपा सागर प्रभु, जिनकी कृपा को प्राप्त कर स्वयं भगवती कृपा भी नहीं अघाती अर्थात् और अधिक की आकांक्षा करती है, वे मेरी सब बातों को सब प्रकार से सुधारेंगे।
भगवान श्री राघवेन्द्र अहेतु की कृपा करने वाले हैं। उनकी कृपा किसी हेतु को लेकर नहीं होती। वे तो सहज कृपालु हैं। वे स्वाभाविक रूप से ही सभी भूत प्राणियो पर कृपा करते हैं। वे कृपा की साक्षात् मूर्ति हैं और उन कृपामय की कृपा अनवरत् रूप से सब पर बरसती रहती है। उस अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित कृपाधारा में सभी डुबकी लगा सकते हैं तथा लाभ उठा सकते हैं। भगवान की जीवमात्र पर बरसती कृपासुधा का सबसे बड़ा और ज्वलन्त उदाहरण मानव शरीर की प्राप्ति है। "कबहुँक करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही।" प्रायः सभी जीवों से नित्य इतने पाप कर्म होते रहते हैं कि उनसे निस्तार पाना करोडों वर्ष में भी संभव नहीं, फिर भी उन पाप कर्मों की ओर ध्यान न देकर प्रभु अपने कृपामयी प्रकृति के अनुरूप मानव देह प्रदान कर हर एक को भगवत्प्राप्ति अथवा मोक्ष का अवसर देते हैं।
कृपा को माया भी कहते हैं। कृपा और माया पर्यायवाची शब्द हैं। माया ही भगवती सीता है। माया ईश्वर से भिन्न नहीं, अज से अजा भिन्न नहीं। अतः, देवाधिदेव परात्पर पुरुष भगवान श्रीराम से परमाद्या मूल प्रकृति भगवती सीता भिन्न नहीं। जिस प्रकार वाणी से अर्थ भिन्न नहीं, जल से तरंग या लहर भिन्न नहीं, चन्द्र से चन्द्रिका भित्र नहीं, उसी प्रकार भगवान राम से माया रूपी सीता भिन्न नहीं। कहने में दोनों भिन्न- भिन्न प्रतीत होते हैं, परन्तु यथार्थतः दोनों एक हैं। जिस तरह भगवान राम कल्याण के दाता तथा सहज कृपालु हैं यानि अहेतुकी कृपा करने वाले हैं, तद्वत जगजननी सर्वश्रेयस्कर भगवती सीता भी कृपा की मूर्ति ही हैं। अतः, भगवती भास्वती कृपादेशी स्वयं कल्याणकारिणी जगन्माता सीता जी ही हैं। सहज ही बिना हेतु कृपा करन उनका स्वभाव ही है। वे भगवत्कृपा की साकार प्राणमयी प्रतिमा हैं। उनका कृपापूर्ण भाव भक्त और भगवान दोनों को आह्लादित कर देता है। वे करुणानिधान प्रभुद्ध कृपा भंडार को प्राणिमात्र के कल्याण के लिए उदार हृदय से सर्वदा लुटाती रहती है। कृपारूपिणी जगजननी सर्व कल्याणकारिणी जानकी जी करुणार्द्र हृदय से भगवत्कृर रस निरंतर वितरण करते हुए कभी नहीं अघाती।
जिस तरह स्वभावी से स्वभाव भिन्न नहीं, उसी तरह पुरुष से प्रकृति भिन्न नहीं जैसे कृपानिधान परमानन्ददाता भगवान राम नित्य व्यापक व अनन्त हैं, वैसे है उनकी कृपा भी नित्य अनन्त व सर्व व्यापक है। अतः, उनकी कृपा सम्पूर्ण विश्वः चर-अचर पर बिना किसी भेदभाव के निरंतर बरसती ही रहती है। चिद्रूपा भगवत भास्वती कृपादेवी उस कृपारस को निरंतर लुटाते हुए कभी नहीं अघाती, इसलि कि वे कल्याणकारिणी जगदम्बा जो हैं। पुत्र, कुपुत्र हो सकता है, परन्तु माता कुमाल नहीं होती। वह सदा सर्वदा अपनी संतान का कल्याण ही चाहती है और उस पर कृ करती ही रहती है।
भक्तवत्सल करुणानिधान भगवान राघवेन्द्र अपने जनों पर तो कृपा करते ही परन्तु उनमें विलक्षणता यह है कि शत्रुओं पर भी कृपा करते हैं। उनके शत्रुगाए क्योंकि वे बैरी हैं और उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, उनकी अहेतु की कृपादृष्टि से वंचि नहीं रहते। उनकी सतत् प्रवाहशीला सहज कृपा सर्वकालिक है और वह साधनों निर्भर नहीं करती। वह अकारण ही सब पर बरसती रहती है, क्योंकि वह देश का वस्तु और व्यक्ति से परे है। वह सर्वरूपों में सर्वत्र प्रकाशित होती है। कृपा और कृपा दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं। राक्षसराज रावण श्रीराम का नाम ही मिटा देना चाहता उसने श्रीराम एवं लक्ष्मणजी को मार डालने के लिए घमासान युद्ध किया। पररू रणभूमि में जब उसके रथ व सब आयुध विनष्ट हो गये और वह मरणोन्मुख हो गर तब दयालु प्रभु के हृदय में करुणा का संचार हो गया और वे रावण से बोले - (वाल्मीकि रामायण) कि आज तुमने बडा भयंकर युद्ध किया है और मेरे बड़े-बड़े वीरों को आहत भी कर दिया है, परन्तु तुम बहुत थक गये हो और अस्त्र-शस्त्र हीन हो गये हो। ऐसी निस्सहाय हालत में मैं तुमको मारना नहीं चाहता, तुम लंका में जाकर विश्राम करो और स्वस्थ होकर तथा आयुधों से सुसज्जित होकर मेरे से आकर युद्ध करो और फिर मेरे बल को देखो। ऐसी दया, ऐसी कृपा क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है, ऐसी दयालुता, ऐसी कृपावत्सलता कृपा के सागर भगवान राम में ही देखी जाती है। वे तो साक्षात् कृपा की मूर्ति ही हैं। उनकी कृपा ऐसी अहेतु की है कि जीवनपर्यन्त दुष्कर्म करने वाले राक्षसों एवं असुरों को भी जिन्होंने भगवान के विरुद्ध रण में तन-त्याग किया, अपना परमधाम प्रदान किया। इसलिए कहा है- "जासु कृपा नहिं कृपा अघाती।" कितना सार्थक व उपयुक्त विशेषण है ।।३।।
राम सुस्वामि कुसेवक मोसी । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ।।
लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती । बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ।।
।। इति श्री राम महिमा समाप्त ।।
3. मनु शतरूपा बरदान
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् ।
यत्कृपामहतं वन्दे परमानंद माधवम् ।।
स्वायंभू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनूपा ॥
दंपति धरम आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह कै लीका ॥
नृप उत्तानपाद सुत तासू । ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासू ॥
लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही । बेद पुरान प्रसंसहि जाही ॥
देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी ॥
आदि देव प्रभु दीन दयाला । जठर घरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥
सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्त्व बिचार निपुन भगवाना ॥
तेहि मनु राज कीन्ह बहुकाला । प्रभु आयसु सबबिधि प्रतिपाला ॥
दोह-होइ न विषय बिराग भवन बसत भा चौथपन ।
हृदयें बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरिभगति बिनु ।।142||
बरबस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥
तीरथबर नैमिष बिख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥
बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहँ हियँ हरषि चलेउ मनु राजा ॥
पंथ जात सोहहिं मतिधीरा । ज्ञान भगति जनु घरे सरीरा ॥
पहुँचे जाइ घेनुमति तीरा । हरषि नहाने निरमल नीरा ॥
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी । घरम धुरंधर नृपरिषि जानी ॥
जहें जहँ तीरथ रहे सुहाए । मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥
कृस सरीर मुनिपट परिधाना । सत समाज नित सुनहिं पुराना ॥
दोहा - द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग ।
बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ||143||
करहिं अहार साक फल कंदा । सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा ।।
पुनि हरि हेतु करन तप लागे । बारि अधार मूल फल त्यागे ।।
उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ।
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतहिं परमारथबादी ।।
नेति नेति जेहि बेद निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥
संप्रभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना ।।
ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहहीं। भक्त हेतु लीला तनु गहई ॥
जौं यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ।।
दोहा-एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार ।
संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर अधार ।।144||
बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ । ठाढ़े रहे एक पद दोऊ ॥
बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आये बहु बारा ।।
मागहु बर बहु भाँति लोभाए । परम धीर नहिं चलहिं चलाए ।।
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा ।।
प्रभु सर्बग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी ।।
मागु मागु बरु भैनभ बानी। परम गभीर कृपामृत सानी ।।
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवन रंध्र होइ उर जब आई ।।
हष्ट पुष्ट तन भए सुहाए । मानहुँ अबहिं भवन ते आए ।।
दोहा-श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात ।
बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ।।146।।
कानों से प्रभु के अमृतमय वचन सुनकर महाराज मनु इतने प्रसन्न हुए और उनका शरीर इतना पुलकायमान हो गया कि उनका प्रेम उनके हृदय में नहीं समा रहा था। वे दंडवत कर बोले ...
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु । बिधि हरि हर बंदित पद रेनू ।।
सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ।।
हे सेवकों के कल्पतरु स्वरूप प्रभु! हे भक्तों के कामधेनु! आपके चरणों की रज की वंदना ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं। आप सबके वंदनीय और पूजनीय हैं। हे शरणागतों के रक्षक! हे अखिल चराचर के स्वामी! सुनिये, आप सेवा (भजन) करने से सब को सुलभ हैं और सब को सुख देने वाले हैं 111, 211
जौं अनाथ हित हम पर नेहू । तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू ।।
जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि यतन कराहीं ॥
जो भुसुंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥
हे अनाथों के हितकारी प्रभु! यदि आपकी हम पर दया है तो प्रसन्न होकर हमे यह वर दीजिये कि आपका जो स्वरूप शिवजी के हृदय में बसता है, जिस स्वरूप के दर्शन के लिए मुनि गण यत्न करते हैं, जो स्वरूप काकभुशुंडि जी के मन रूपी मानसरोवर में हंस रूप से निवास करता है और वेद जिसका गुणगान करते हैं कि जो निर्गुण होते हुए सगुण है और सगुण होते हुए निर्गुण हैं, उसका हम नेत्र भरकर दर्शन करें। हे शरणागतों के दुःख दूर करने वाले स्वामी! आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम आपके रूप को जी भर के देखें।
शंकर जी के हृदय में भगवान का कौन-सा रूप बसता है? स्वयं महादेव जी अपने श्रमुख से गिरिराज कुमारी के प्रति कहते हैं-
बन्दौं बाल रूप सोइ रामू। सब सिघि सुलभ जपत जेहि नामू ।।
फिर भगवान राम का जन्म महोत्सव वर्णन करते हुए वे कहते हैं -
औरउ एक कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ।।
कागभुसुंडि संग हम दोऊ । मनुज रूप जानइ नहिं कोऊ ॥
परमानंद प्रेम सुख फूले । बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥
इस कथन से ज्ञात होता है कि शिवजी को भगवान राम का बाल रूप अधिक प्रिय है और वही बाल रूप सदा उनके मन में बसता है।
अब भुशुंडी जी के मन मानस में जो रूप निवास करता है, उसे भी उन्हीं के मु से सुनिये -
जन्म महोत्सव देखउँ जाई । बरष पाँच तहँ रहऊँ लोभाई।
इष्टदेव मम बालक रामा । सोभा बपुष कोटि सत कामा ।।
निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी ॥
इस तरह सिद्ध होता है कि महात्मा काकभुशुंडी भी भगवान राम के बाल रूप के पुजारी हैं। मुनिगण जैसे वाल्मीकि, शरभंग, सुतीक्ष्ण, भरद्वाज, अगरत्य, वशिष्ठ आदि भी सब परात्पर भगवान के राम रूप के भक्त थे और उसी रूप के दर्शन के अभिलाषी थे। अतः, दम्पत्ति ने उसी विश्व विमोहन राम रूप के दर्शन की इच्छा की जिसे भगवान ने पूर्ण किया और उन्हें बाल चरित का सुख भी प्रदान किया।
दंपति बचन परम प्रिय लागे । मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे ।।
भगत बछल प्रभु कृपानिधाना। बिस्बास प्रगटे भगवाना ।।
भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले, दया के सागर, सारे चराचर में रमने वाले, सर्वव्यापक भगवान को राजा रानी के विनम्र और मधुर वचन बहुत ही प्रिय लगे। उनके प्रेम से सने हुए कोमल वचनों को सुनकर सारे चराचर में ओत-प्रोत रहने वाले प्रभु प्रगट हो गये।
दोहा-नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम ।
लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि-कोटि सत काम ||146||
सरद मयंक बदन छबि सीवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ।।
अघर अरुन रद सुन्दर नासा । बिधुकर निकर बिनिंदक हासा ।।
नव अंबुज अंबक छबि नीकी । चितवनि ललित भावतो जी की ।।
भृकुटि मनोज चाप छबि हारी । तिलक ललाट पटल दुति कारी ।।
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा ।।
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला । पदिकहार भूषण मनि जाला ।।
केहरि कंघर चारु जनेऊ । बाहु विभूषन सुन्दर तेऊ ।।
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥
दोहा-तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीनि ।
नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भर्वैर छबि छीनि ।।147।।
पद राजीव बरनि नहिं जाहीं । मुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह माहीं ॥
बाम भाग सोभित अनुकूला । आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला ।।
जासु अंस उपजहिं गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ।।
भृकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥
छबिसमुद्र हरि रूप बिलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥
चितवहिं सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥
हरष बिबस तन दसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा । तुरत उठाए करुनापुंजा ॥
दोहा-बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि ।
मागहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ।।148।।
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । घरि धीरजु बोले मृदु बानी ॥
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे ।।
एक लालसा बड़ि उर माहीं । सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहिं निज कृपनाई ॥
जथा दरिद्र बिबुध तरु पाई । बहु संपति मागत सकुचाई ।।
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई । तथा हृदय मम संसय होई ॥
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ।।
सकुच बिहाइ मागु नृप मोही । मोरें नहिं अदेय कछु तोही ॥
दोहा - दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ ।
चाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ||149||
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥
आपु सरिस खोजौं कहें जाई । नृप तव तनय होब मैं आई ॥
सतरूपहि बिलोकि कर जोरे । देबि मागु बरू जो रुचि तोरे ॥
जो बरू नाथ चतुर नृप मागा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई । जदपि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥
अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥
जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिं जो गति लहहीं ||
दोहा- सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु ।
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ।।150||
हे नाथ! जो आपके अनन्य (खास) भक्त हैं, वे जो सुख पाते हैं और जो गति प्राप्त करते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, अपने चरण कमलों में वही स्वाभाविक अनुराग, वही विवेक (ज्ञान) और वही रहनि, हे प्रभु! हमें कृपा करके दीजिये ....
महारानी शतरूपा प्रार्थना करती हैं, हे प्रभो! हमें वही सुख जिसकी चाह अनादिकाल से जीव मात्र को है, जिसे पाकर पाना कुछ भी बाकी नहीं रह जाता और जिसे पाकर तीनों काल की स्मृति का लोप हो जाता है, वही अविरल भक्ति, जिसे बडे-बडे योगि मुनि ढूँढते और प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जिसे पाकर वर्णाश्रम धर्म का त्याग हो जाता है, जिसे प्राप्त कर भक्तों का मद और माया नाश हो जाता है, जो स्वतंत्र है, अनुपम है और संतों की कृपा से प्राप्त होती है, प्रभु चरणों में वही सहज सनेह जिससे किसी वस्तु की कामना नहीं रह जाती और जो संसार सागर तरने के लिए नौका रूप है, वही विवेक जिससे किसी में किसी भी प्रकार का कोई गुण या दोष कभी भी न दिखाई दे और ऐसी रहनी जैसे संत महात्माओं की होती है, कृपा कर देवें।
वह कौन-सा सुख है जिसकी खोज अनादि काल से जीव मात्र को है? वह कैसा सुख है, जिसके लिए “योगी यतन करहिं जेहि लागी। भूप राज तजि होहिं विरागी।" वह कैसा सुख है, जिसको प्राप्त करने के लिए जीव मात्र अनादि काल से संसार में नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों में रत हैं और जिसे प्राप्त किये बिना जीव कभी सुखी नहीं होता? वह कौन-सा सुख है, जिसको बिना प्राप्त किये जीव का आवागमन बंद नहीं होता? वह सुख है आत्म सुख, ब्रह्म सुख, निज सुख या निजानंद, नित्य सुख या नित्यानंद, ब्रह्मानंद, स्वरूपानंद। वह ऐसा सुख है, जिसका कभी क्षय नहीं और जो निरंतर प्राप्त होता रहता है, जो इन्द्रियों से परे है और मन वाणी की ५ के बाहर है। जीव को क्षण प्रति क्षण सुख तो मिलता रहता है, परन्तु वहन्द्रिय जन्य होने से क्षणिक है, आगमापायी है, उससे जीव को शांति नहीं मि. ती। जीव को शाांति तो तभी मिलती है, जब उसे सुख का भण्डार, आनंद का स र, नित्यानंद की प्राप्ति होती है। नदियाँ तभी शांत और स्थिर होती है जब उन्हें अगाध जल का अपार भण्डार (समुद्र) मिलता है। कहा भी है "सरिता जल जलनिधि म्हुँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हरि पाई।" जिस प्रकार नदियाँ सागर में पहुँचकर शांत हो जाती है, उसी प्रकार बोधवान पुरुष यानि भक्त जन अपने स्व-स्वरूप भगवान आत्मा को प्राप्त कर, उसका दर्शन या अनुभव कर शांत और सुखी होते हैं। इसी ब्रह्म सुख, नित्य सुख या आत्मानंद की याचना महारानी शतरूपा ने भगवान से की।
समस्त प्राणी मात्रका लक्ष्य नित्य सुख, चिर सुख या ब्रह्मानंद की प्राप्ति है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त प्राणी नित्य सुख की खोज में रहता है। उस नित्य सुख की प्राप्ति के लिए वह शुभाशुभ कर्म करता रहता है। जब उसे नित्यानंद प्राप्त हो जाता है, तब उसका शुभाशुभ कर्म करना बंद हो जाता है। नित्यानंद की प्राप्ति के लिए ही समस्त कर्म, नाना प्रकार के साधन, यम, नियम, व्रत आदि किये जाते हैं। जिस आत्मानंद को चोर चोरी में, शराबी शराब में, दुराचारी दुराचार में ढूँढ़ता है, उसी नित्यानंद को तपस्वी तप में, योगी योग में, संन्यासी संन्यास में, वैरागी वैराग्य में ढूँढ़ता है। उसी सुख की प्राप्ति के लिए पूजा, पाठ, दान, पुण्य, ध्यान, धारणा आदि किये जाते हैं।
इन्द्रिय जन्य या विषय जन्य जितने भी कर्म होते हैं, उनसे जो सुख मिलता है उनका परिणाम दुःख रूप होता है। मन जन्य, वाणी जन्य, कर्म जन्य जो भी सुख मिलता है, वह सुख सच्चा सुख नहीं, क्योंकि उससे अंत में दुःख मिलता है। सुख के अभाव में दुःख है। जब सुख नहीं तब दुःख तो मिलता ही है। वह सुख जिसे पाकर सुख-दुःख दोनों का अभाव हो जाता है, उस सुख की याचना है। जिस क्षणिक सुख का परिणाम दुःख है, उस दुःख से मन दुःखी होता है। जिस दुःख का फल सुख है, उससे मन दुःखी हो जाये, वैसा सुख भी नहीं चाहिये। वह सुख चाहिये जिसमें न सुख हो, न दुःख हो, जो सुख-दुःख से रहित हो अर्थात् परिणामहीन हो। जो सुख आगमापायी है, उसमें हँसना या रोना होता है। वह सुख जो सुख-दुःख रहित हो अर्थात् परिणाम रहित हो, वही नित्य सुख है, आत्म सुख है। बोध शून्य मनुष्य इस आत्म सुख में शून्यता का अनुभव करता है। वह यथार्थ में सुख-दुःख से परे पद है जो आनंद का सागर है और जिसे प्राप्त कर पाने वाले का व्यक्तित्व ही खतम हो जाता है। जैसे समुद्र को पाकर नदियों को यह याद नहीं रहती कि आज से पहिले हम क्या थीं, उसी प्रकार नदी रूपी जीव को आनंद सागर की प्राप्ति होने पर यह याद नहीं रहती कि पहिले वह ज्ञानी था या अज्ञानी, बद्ध था या मुक्त। वही सुख है जहाँ न सुख है, न दुःख, न शोक है, न मोह, न ज्ञान है, न अज्ञान, न हर्ष है, न विषाद और न किसी प्रकार के अन्य विकार। जिस सुख को पाकर प्राप्ति अथवा अप्राप्ति के विकल्पों का नाश हो जाता है, वही सुख, वही आत्म सुख वही आत्मानंद की चाह है।
जिस सुख की प्राप्ति के लिए जीव अनादि काल से अनन्त साधनाएँ करते आ रहा है, उसी सुख की प्राप्ति के लिए कोई 'है' को पूजता है तो कोई 'नहीं' को मानता है। जब वह सुख प्राप्त हो जाता है, तब जीव न किसी की निंदा करता है और न स्तुति करता है। तब उसके सब साधनों का अंत भी हो जाता है। जब साधनों का अंत हो जाता है, तब फिर स्तुति या निंदा किसकी करेगा और क्यों करेगा? जहाँ पहुँचकर जिस आनंद सागर को प्राप्त कर, जीव की पुनरावृत्ति संसार में नहीं होती, उस सुख की चाह है। जब उसे ब्रह्म सुख मिल गया तो वह विषय जन्य क्षणिक सुख के पीछे क्यों दौड़ेगा? मृग रुपी मन को जब वास्तविक जल रूपी आत्म सुख मिल गया तब फिर वह मृगतृष्णा रूपी कामनाओं के पीछे क्यों दौड़ेगा? अपने अंदर के खजाने को न जानने के कारण कस्तूरी मृग इधर-उधर जंगल पहाड़ों में सुगंधि के पीछे पागल बने फिरता है। परंतु जब कभी उसकी नाक अपनी नाभि की ओर चली जाती है और जब उसे अपने ही अंदर सुगंध के भण्डार का पता चल जाता है, तो उसका भटकना बंद हो जाता है। उसी प्रकार जीव अपने ही अंदर आत्म सुख रूपी आनंद सागर को पाकर विषय सुख रूपी बाहरी सुगंध के पीछे दौड़ना छोड़ देता है। जब सद्गुरु की " कृपा से वह जान जाता है कि आनंद का सागर उसी के अंदर हिलोरें मार रहा है, तब उसका भटकना अथवा साधन बंद हो जाता है। जिस सुख को पाकर मन अमन हो जाता है, चित्त चित् हो जाता है और बुद्धि बोध हो जाती है, उसी सुख की याचना है।
जिस सुख की याचना महारानी शतरूपा कर रही है और जिस सुख के लिए योगी जतन करहि जेहि लागी। भूप राज तजि होहि बिरागी।" - वह क्या एक स्थान में मिलता है? नहीं, वह तो सारे चराचर में व्याप्त है कण-कण में लबालब है। वह समस्त जगत् प्रपंच में परिपूर्ण है। वह एक देशीय न होकर सर्वत्र ओत-प्रोत है, सारे विश्व की आत्मा है, सारे चराचर का अस्तित्व है। वही तुम्हारे अंदर भी है और यात्रा की मंजिल भी तुम्हारे अंदर है। वही आत्मा सुख का भण्डार है, आनन्द का सागर है और उसी आत्म सुख की याचना महारानी ने की है।
जिस सुख का फल दुःख है, वह सुख अप्राप्ति की प्राप्ति है। वह सुख साधन जन्य है और क्षणिक है। जो प्राप्ति की अप्राप्ति है, जो सुख न सुखानुभूति है और न दुःखानुभूति है, वह कृपा साध्य है। महारानी जी ने जिन छह वस्तुओं की याचना की है यानि सुख, गति, भक्ति, चरण सनेह, विवेक और संत रहनी वे सभी कृपा साध्य है, वे साधन साध्य नहीं हैं। वे संतों की कृपा से अथवा भगवान की कृपा से प्राप्य हैं। उनके लिए मन, वचन, कर्म किसी के द्वारा भी साधन नहीं हो सकता। उनके लिए संत या भगवान की कृपा ही एकमात्र साधन है। वे प्राप्ति की प्राप्ति है। यद्यपि वे सर्वदा प्राप्त हैं, परन्तु जीव अपनी अज्ञानता के कारण उन्हें भूला हुआ है। संत महात्मा की कृपा से जब वह आत्म सुख का अनुभव कर लेता है, तब वह निहाल हो जाता है और उसका भटकना बंद हो जाता है।
मन, वचन, कर्म द्वारा जितने भी कार्य होते हैं वे अपने आप 'मैं' को कुछ मान कर ही होते हैं और उनका फल दुःखानुभूति है। मन, वचन, कर्म द्वारा होने वाले समस्त कार्य अपने आप 'मैं' आत्मा को जब कुछ न मानकर होते हैं, तब अनुभूति की यानि 'मैं' आत्मा की अनुभूति होती है। अपने आप 'मैं' आत्मा को कुछ न मानना ही आत्मा का जानना है और जो 'मैं' आत्मा हूँ, वही सुख-दुःख से परे है। उसका अनुभव ही सुख-दुःख से परे ब्रह्म सुख है, आत्मानंद है। जीवों के सारे कार्य स्वरूप स्थिति में होते हैं, चाहे वे अनजाने में ही क्यों न हों। इस प्रकार सारा चराचर स्वरूपस्थ है, समाधिस्थ है। इसलिए वह प्राप्ति की प्राप्ति है, क्योंकि सबको प्राप्त है। परन्तु, अज्ञानी इसे अप्राप्ति की प्राप्ति मानकर उसके लिए अनादि काल से साधन करते हुए भटक रहे हैं। संत महात्मा उसे क्षण मात्र में लखा देते हैं। जब मैं आत्मा अपने आप को कुछ मानता हूँ, तभी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विषयों का विकल्प होता है। परन्तु, जब मैं विषयों का अनुभव करने चलता हूँ, तब न तो मान्यता रहती है और न ही विषयों का अनुभव होता है। केवल 'मैं ही मैं' शेष रह जाता हूँ और केवल मुझ आत्मा का ही अनुभव होता है। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल में कभी भी न कुछ हुआ था, न हो रहा है और न होगा। था तो मैं आत्मा, हूँ तो मैं आत्मा और रहूँगा तो मैं आत्मा। यही निष्ठा आत्म सुख है, आनंद का सागर है और इसी विशुद्ध आल सुख की याचना महारानी जी ने की है।
अपने आप 'मैं' आत्मा को कुछ मानना जीव देश का कार्य है और कुछ न मानना आत्म देश है। जीव देश में प्रपंच है, राग-द्वेष है, हर्ष-शोक है, सुख-दुःख है, हानि-लाभ है, पुण्य-पाप है, धर्म-अधर्म है, इत्यादि अनेकों द्वन्द्व हैं। परन्तु, आत्म देश में इन सबका अत्यंताभाव है, केवल है तो भगवान 'मैं' आत्मा। 'मैं जीव हूँ' यह विकल्प ही अकेला केवल जीव नहीं है, अपितु 'मैं' और 'हूँ' के बीच में जो कुछ भी आता है सभी जीव देश के हैं, जीव देश में हैं और जीव देश ही है। इसी अनुभूति से कर्मजाल से छुटकारा मिलता है। यदि वस्तुतः, कर्मजाल होता तो उससे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता था। यथार्थ में कर्मजाल मान्यता है, है ही नहीं। इसी की अनुभूति आत्म सुख है और इसी के लिए महारानी शतरूपा की याचना है।
महारानी जी ने छह चीजों की याचना की और उन सबकी प्राप्ति के लिए कृपा करने की प्रार्थना की। इससे यह सिद्ध होता है कि सब साधन साध्य न होकर कृपा साध्य हैं। साधन द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वह कृत्रिम, अनित्य और क्षणिक है, वह नाश को प्राप्त होता है। परन्तु, जो सुख बिना किसी प्रकार के साधन के स्वाभाविक रीति से प्राप्त हो या संत अथवा भगवत् कृपा का फल हो, वह सहज सुख है। ऐसा ही सहज सुख, सहज गति, सहज भक्ति, सहज सनेह, सहज विवेक और सहज रहनी की याचना है। यह सहज सुख, आत्म सुख या ब्रह्म सुख आत्मा ही है। अनित्य या क्षणिक सुख का तो अनुभव होता है, परन्तु आत्म सुख या ब्रह्मानन्द तो आत्मा ही है। जिस सुख को पाकर मन सुखी हो, वह कृत्रिम या क्षणिक सुख है, उसका अनुभव 'मैं' आत्मा करता हूँ और जिस सुख को पाकर मन अमन हो जाये, चित्त-चित् हो जाय और बुद्धि बोध हो जाय, वह सहज सुख है, आत्म सुख है। इस सहज सुख में सुखानुभूति अथवा दुखानुभूति का अभाव रहता है। सुखानुभूति और दुःखानुभूति के अभाव का जो भाव है वह सहज सुख है।
मन का स्वरूप है चंचलता। लय और विक्षेप भी मन के स्वरूप हैं। मन की चंचलता का नाम ही विक्षेप है। नींद आ जाना मन का लय है। किसी विषय के अनुभव काल में यदि मन विक्षिप्त हो जाय तो वह कार्य नहीं हो सकता। यदि मन लय हो जाये तो नींद आ जाने पर भी कार्य नहीं हो सकता। कथा के श्रवण काल में या सिनेमा देखते समय मन का न तो लय होता है और न विक्षेप। वहअमन हो जाता है अर्थात् - मन का कहीं पता नहीं रहता। मन क्यों अमन हो जाता है? इसलिए कि मन नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जो कुछ है वह मैं आत्मा। 'मैं' हूँ, इसलिए मन नहीं है। यदि 'मैं' अमुक (मान्यता) हूँ, तब तो मन है और यदि 'मैं' हूँ तो मन नहीं है। 'मैं' कैसा = हूँ? 'मैं' जैसा हूँ, वैसा ही हूँ, 'मैं' जहाँ हूँ वहीं हूँ, 'मैं' जो हूँ वही हूँ। 'मैं' मन, वाणी = का विषय नहीं हूँ। वाणी नहीं कह सकती कि 'मैं' कैसा हूँ। फिर भी 'मैं' हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, 'मैं' हूँ। मुझ भगवान आत्मा को मन, बुद्धि आदि की जरूरत = नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसलिए मुझ आत्मा को अनुभव करने के लिए - किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। 'मैं' नित्य ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझ आत्मा का ज्ञान = सहज ज्ञान है। जब 'मैं' स्वयं अपने आप को कैसा हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ आदि वाणी = द्वारा व्यक्त करने में असमर्थ हूँ तो दूसरे मेरा वर्णन कैसे कर सकते हैं? 'मैं' मन वाणी = से परे हूँ, केवल सत्ता मात्र अस्तित्व मात्र शेष रह जाता है। सोइ अनुभूति, सोइ सुख।
सोइ सुख क्यों कहा? सु माने सुन्दर और ख माने आकाश। इस तरह सुख का - अर्थ होता है सुन्दर आकाश, निर्विकार, निर्लेप आकाश। मैं आत्मा आकाशवत् सुन्दर, निर्लेप, निर्विकार हूँ। मुझ आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं, 'मैं' सहज - सुख स्वरूप हूँ। जिस देश में 'मैं' (आत्मा) हूँ, इस संज्ञानुभूति का भी अभाव है, वह आत्म देश है। वही सहज पद, सहज सुख, सहज समाधि, सहजानंद, ब्रह्मानंद है। 'मैं' हूँ- इस संज्ञा की अनुभूति तो जागृत अवस्था में जब मन, बुद्धि, चित्त रहता तय होती है, परन्तु सुषुप्ति अवस्था में जब मन नहीं रहता तब इसकी अनुभूति नहीं होती। इसलिए इस संज्ञा की अनुभूति का अभाव सहज सुख है। 'मैं' हूँ इस संज्ञा की भी अनुभूति की अभावानुभूति किसी विषय के अनुभव काल में ही होती है। जब 'मैं' हूँ, इस संज्ञा की भी अनुभूति नहीं, तब फिर शब्दादिक शब्दों की अनुभूति कैसे होगी? वहाँ तो केवल अस्तित्व मात्र शेष रह जाता है। वही सहज सुख की याचना है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम की महिमा का बखान करते हुए कहा है -
राम सरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर ।
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ।।
'मैं' आत्मा भगवान राम इस प्रकार वर्णनातीत है -
किसी को बंधन से निकलने की इच्छा क्यों नहीं होती? इसलिए कि उसका वह बन्धन उसका स्वतः का माना हुआ है। क्योंकि, कोई दूसरा उसे बांधे नहीं रहता, वह अपने को बंधनयुक्त नहीं समझता। वह जानता है कि वह जब चाहेगा तब निकल सकेगा। परन्तु, जब यह मालूम होता है कि किसी दूसरे ने उसे बंधन में डाला है, तब उसे घबराहट हो जाती है, उसे दुःख होता है और वह उससे निकलने का प्रयल करता है। स्वतः के माने हुए बंधन में घबराहट नहीं होती, उसमें निश्चितता रहती है। वही सहज सुख।
किसी ने देखने, सुनने, हँसने, रोने, खाने, पीने का अभ्यास नहीं किया। क्रियायें उसकी स्वाभाविक होती हैं। कोई भी प्राणी सहज ही देखता है, सहज है सुनता है, सहज ही खाता है, सहज ही पीता है आदि। मन, वचन, कर्म द्वारा होने वाले कार्य सब कृत्रिम होते हैं या सहज? वे सब कार्य सहज कर्म हैं, क्योंकि उन कर्म के करने का अनुभव मुझे नहीं होता। यदि मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ या खा-द रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ और उस कार्य के करने का मुझे भान होता है, तब जो कुः मैं करता हूँ, वह कृत्रिम है। पर यदि जब कुछ भी अनुभव या भान न हो तो वही सहा कर्म है। वही सहज कर्म सुख है और जो कर्म करता है वह भी सहज है। जितने कर्म सब हो रहे हैं, वे सब सहज अवस्था में ही हो रहे हैं। सहज द्वारा सहजावस्था ही सहज कर्म होते हैं। जब कर्म सहज, सब अवस्था सहज, तब कर्म का करने वाल भी सहज होगा। जो सुख सहज है, उसे साधना द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भी सहज ही प्राप्त होगा इसलिए सोइ सुख।
जब मैं आत्मा अपने आप को कुछ मान लेता हूँ कि मैं जीव हूँ या मैं देह हूँ आदि। तब भी मुझ आत्मा का सहजपना कहीं नहीं चला जाता। अपने आप को कुछ मान लेने से तो मैं वह नहीं हो जाता। यदि मानने से मैं वैसा हो जाऊँ, तो उसकी स्मृति मुझे सदा बनी रहती। परन्तु, वैसा होता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि मानने के बाद भी मैं वही रहता हूँ, जैसा मानने के पहिले था। वाणी द्वारा जो कुछ व्यक्त किया जाता है वह सहज नहीं है, क्योंकि वह सोच-समझकर बोला जाता है और बोलने वाले को उसका भान रहता है। परन्तु, देखने-सुनने का कर्म सहज है। जिस अवस्था में देखा सुना जाता है, वह अवस्था सहज है। उसके लिए कोई साधन नहीं किया जाता इसलिए देखने-सुनने वाला भी सहज है। मन, वचन, कर्म द्वारा रात-दिन जो व्यवहार होते हैं वे सब व्यवहार सहज और अवस्था भी सहज, इसलिए व्यवहार करने वाला भी सहज। इस सहजावस्था में न सुख का अनुभव होता है और न दुःख का। वह सुख-दुःख से परे अवस्था है। वह सहजावस्था ही सहज सुख है। सहजानुभूति में सहज सुख का अनुभव निहित है। उसका अनुभव कर लेने पर ही सहज सुख की अनुभूति होती है। यह जो सहज अवस्था की अनुभूति है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यही सहज सुख है, यही सहजावस्था है, यही सहजानन्द है। इस अनुभूति में देश, काल, वस्तु, सुख-दुःख आदि का अभाव रहता है। इसका अनुभव सहज, इसकी अवस्था सहज, इसका अनुभवकर्त्ता सहज, इसका अनुभव कराने वाला सहज, इसका सब कुछ सहज है। यही सहज सुख है, सहज ही सुख है और इसी सहज सुख के लिए महारानी शतरूपा की याचना है।
2. सोइगति -
गति के चार अर्थ होते हैं गमन, मोक्ष, ज्ञान और प्राप्ति। यहाँ पर गति का अर्थ मोक्ष या मुक्ति लिया गया है। कैसी गति ? कैसी मुक्ति? स्वाभाविक गति या सहज मुक्ति। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो बंधना चाहता हो। सब ही मोक्ष चाहते हैं। सब ही स्वतंत्रता की बाँछा करते हैं। प्राणीमात्र मुक्त रहना चाहते हैं। एक मुक्ति होती है बंध की अपेक्षा और दूसरी होती है स्वाभाविक। बंध की अपेक्षा जो मुक्ति है वह कृत्रिम है, साधन जन्य है और साधन से मिलती है। दूसरी मुक्ति स्वाभाविक मुक्ति है, यह साधन जन्य न होकर कृपा साध्य है। अपने आप में आत्मा को कुछ मान लेना यही बंधन स्वरूप है और अपने आप को कुछ न मानना जैसे का तैसे जानना, यही मोक्ष है।
निरालंबोपनिषद में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, परमात्मा, जाति, कर्म-अक ज्ञान-अज्ञान, बंध-मोक्ष, गुरु-शिष्य, विद्वान-मूर्ख, संन्यासी आदि की व्याख की गयी है। सब धर्मों को परित्याग करके निरहंकार होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुर की शरण में जाकर "अहं ब्रह्मास्मि", "तत्त्वमसि', सर्व खलुमिदं ब्रह्म नेहनानाकि किंचन इत्यादि। महावाक्यों द्वारा बार-बार विचार करके अपने स्वरूप भगवान आव को निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में अर्थात् अपने स्वरूप आत्मा में स्थित होका जो स्वतंत्र विचरता है, वही संन्यासी है, वही पूज्य है, वही पंडित है, वही परमहंग है, वही ब्राह्मण है, वही अवधूत है और वही मुक्त है। बंध की अपेक्षा जो मुक्ति है, क मुक्ति नहीं चाहिए, स्वाभाविक मोक्ष चाहिए। हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि है उसक खुलना ही मोक्ष है। बंध है-ऐसा मानकर ही बंधन से छुटकारा पाने का संकल्प होन है, परन्तु महारानी शतरूपा की याचना तो सहज मोक्ष अर्थात् स्वाभाविक गति लिए है। बंधन यदि वास्तविक है तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य क नाश नहीं होता। बंधन यदि असत्य है तो मान्यता होने के कारण वह है ही नहीं, फि छुटकारा या मुक्ति किससे? अभाव रूप पदार्थ से कैसा बंधन और कैसा छुटकारा सत्यासत्य कहना भी दोषपूर्ण है। इसलिए बंधन की धारणा ही गलत है। बंधन तीन काल में है ही नहीं। बंधन का विकल्प ही बंध है और मोक्ष का विकल्प ही मुक्ति है। क और मोक्ष के विकल्पों से रहित जो अवस्था है वही स्वाभाविक मोक्ष है, वही सहर गति है।
यदि ऐसा कहो कि "मैं बद्ध हूँ" तो फिर प्रश्न उठता है कि तुम्हें बांधा किसने यदि कहो कि – 'मैं मुक्त हूँ' - तो फिर किसने मुक्त किया और किससे मुक्त किया मैं अपने आपको नहीं जानता, क्या इसलिए मैं बद्ध हूँ? अपने आपको जो माया ईश न जाने वही जीव है और जो अपने आप को माया का ईश जाने शिव है। तब कौन है, जो अपने आपको माया का ईश न जानने के कारण जीव कहलाता है? जीव तो है नहीं। जानने से शिव और न जानने से जीव नाम पडा है। वह वही है ज जीव है और न शिव है। जब वह वही है तो उसमें न बंध है और न मोक्ष है। बंधन मान्यता में जीव है और मोक्ष की मान्यता में शिव है। बद्ध दशा में जीव और मुक्त दा में शिव। ऐसा जो निश्चय है, ऐसी जो स्थिति है, वही सहज गति है। बंध की अपे मोक्ष है। बंधन के अभाव में मोक्ष का भी अभाव है। उसी तरह जीव के अभाव में रि का भी अभाव है। इसलिए न बंध है और न मोक्ष है। न जीव है, न शिव है। ऐसा निश्चय, ऐसी जो स्थिति, वही सहज गति है।
यदि मैं कहता हूँ में ऐसा हूँ तो ऐसा को जानकर ही तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। तो न तो मैं ऐसा को नहीं जानता और न मैं जैसा हूँ इसको नहीं जानता। मैं दोनों को जानता हूँ। तो फिर अज्ञान कहाँ गया? अज्ञान है ही नहीं। जब अज्ञान नहीं तब बंध भी नहीं। ऐसा जो देश है, ऐसी जो स्थिति है, वही सहज गति है, तो फिर अज्ञान किसमें, अज्ञान है किसको और अज्ञान किस पर? यदि कहो कि मुझ आत्मा में अज्ञान है या मुझ आत्मा को अज्ञान है या मुझ आत्मा का अज्ञान है या मुझ आत्मा पर अज्ञान है, तो क्या 'मैं हूँ' इसका भी अज्ञान किसी को है? जब 'मैं हूँ' इसका अज्ञान किसी को नहीं, तब बंधन कहाँ? जब बंधन नहीं तब मोक्ष भी नहीं। इस तरह बंधन से मुक्ति, मोक्ष से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति और ज्ञान से मुक्ति, यानि सब प्रकार की मान्यताओं से मुक्ति। ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो निश्चय है, वही सहज गति है। यह साधन साध्य नहीं है। यह सबको स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। कोई बद्ध नहीं है, सब मुक्त हैं। सद्गुरु मुक्त को ही मुक्ति लखाते हैं। बद्ध को मुक्ति नहीं दिलाते। जिस प्रकार गधा, घोड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म ही ब्रह्म होता है। ऐसा जो निश्चय है वही सहज गति है।
गति माने मोक्ष और गति माने ज्ञान भी होता है। मुझ आत्मा का जो जानना धर्म है, उसको सीखने के लिए क्या कोई शिक्षक की आवश्यकता होती है या कोई साधन करना पड़ता है? नहीं, यह ज्ञान स्वाभाविक है। मैं आत्मा अनादिकाल से जान रहा हूँ। यदि यह ज्ञान कृत्रिम होता है, तो आज तक उसमें कुछ न कुछ कमी हो ही जाती। परन्तु उसमें कभी कमी नहीं होती, ज्ञान का भण्डार अटूट है। साधन द्वारा प्राप्त ज्ञान यानि सीखा हुआ ज्ञान भूल जाता है। परन्तु, स्वाभाविक ज्ञान मुझ आत्मा का सहज ज्ञान अखंड है, वह कभी नहीं भूलता। मैं कब से जानता हूँ इसे कोई नहीं जानता। इस सहज ज्ञान या स्वाभाविक ज्ञान को ही सहज गति कहते हैं। जब मैं सब जानता हूँ, तब मेरे ज्ञान नापने में कभी कोई कमी नहीं आती, तब फिर अज्ञान कहाँ? "ज्ञान अखण्ड एक सिताबर'। मुझ आत्मा का ज्ञान अखण्ड है। में आत्मा सर्व काल में, सर्व अवस्था में ज्ञान स्वरूप हूँ। संत महात्मा इसी सहज ज्ञान का अनुभव करते हैं। इसी सहज ज्ञान को, सहज पद भी कहते हैं। यही सहज गति है।
निश्चय करते-करते बुद्धि थक जाती है, चिंतन करते-करते चित्त थक जाता है, सोचते-सोचते मन थक जाता है, चलते-चलते पैर थक जाते हैं, देखते सुनते व अन्य काम करते-करते आँख, कान आदि सब इन्द्रियाँ भी थक जाती हैं, परन्तु मैं आत्मा जानते-जानते कभी नहीं थकता, इसलिए मैं आत्मा अखण्ड ज्ञान स्वरूप हूँ। इसी को सहज प्रकाश भी कहते हैं। सहज प्रकाश ही सहज ज्ञान है, भगवान आत्मा है और यही सहज गति है।
जानना क्रिया है। इससे मालूम होता है कि जानने वाला जानने की क्रिया से भित्र है। परन्तु नहीं यथार्थ में ऐसा नहीं है। जिस प्रकार आँख और देखना, कान और सुनना अलग-अलग नहीं, जिस प्रकार स्वभाव से स्वभावी भिन्न नहीं, उसी प्रकार जानने वाला जानने से भिन्न नहीं। इसलिए मुझ आत्मा का जाननापना मुझ आत्मा से भिन्न नहीं। जानना ही मुझ आत्मा का धर्म है, स्वभाव है। छोटे बच्चे को भी ज्ञान है। पैदा होते ही वह देखता है, सुनता है, हँसता है, पीता है इत्यादि। यदि उसे ज्ञानर होता तो वह न तो देखता, न रोता, न हँसता, न पीता इत्यादि कुछ भी कर्म नहीं करता। उसका वह ज्ञान सहज ज्ञान है, इसलिए कि आत्मा अखण्ड ज्ञान स्वरूप है।
'मैं नहीं जानता' - इस बात को मैं जानता हूँ। 'मैं' जानता हूँ' - इसको भी मैं जानता हूँ। जानना और नहीं जानना दोनों को मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप हूँ। यह सहज ज्ञान है और साधन का विषय न होकर कृपा साध्य है। इस पर सबको अधिकार है। मैं बद्ध हूँ, तब भी 'मैं' हूँ। मैं मुक्त हूँ, तब भी मैं हूँ। मैं आत्मा हर हाल में हूँ। 'मैं' आत्मा पर कोई बंधन नहीं, मैं सर्वदा मुक्त हूँ। जब मैं ज्ञान प्राप्त करूँ तब भी मुक्त और न ज्ञान प्राप्त करूँ तब भी मुक्ता बंधन मानना ही बंधन का कारण है। सब स्वाभाविकतः ही मुक्त हैं, ऐसा ज्ञान ही सहज ज्ञान है। जैसा मैं सहज हूँ, जैसा में सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, वैसा ही सब कोई है, न कोई कम है और न कोई ज्यादा है। सब कोई सहज ज्ञान स्वरूप हैं। मैं ज्ञानी हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान के लिए लिखना-पढ़ना, सीखना आदि की जरूरत है। परन्तु 'मैं हूँ' इसके लिए लिखने- पढ़ने, सीखने की आवश्यकता नहीं। यह कृपा साध्य है और इसीलिए महारानी जी याचना की कि 'मोहिं कृपा करि देहु' । यही कृपा साध्य ज्ञान है और यही सहज गति है। इसीलिए कहा गया है -
दुर्लभोविषय त्यागः दुर्लभं तत्वदर्शनम् ।
दुर्लभो सहजावस्था, सद्गुरोः करुणां बिना ।।
फिर कैसी गति ? नदियों की सी गति। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप परित्याग कर समुद्र रूप हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान विवेकी पुरुष नाम रूपर मुक्त होकर दिव्य पुरुष जो परमात्मा है, उसको प्राप्त हो जाते हैं। नदियाँ समुद पहुँचने के पहिले किनारे पर ही नाम रूप का त्याग कर देती हैं। नाम रूप ही तो नदी थी। नाम रूप का त्याग करते ही नदी खतम हो गयी। तब किसने प्राप्त किया, किसको प्राप्त किया और कौन प्राप्त हुआ? यदि नदी बची रहे तो उसे अतीत की याद रहे। जब नदी ही नहीं रही, तब किसको याद रहे? जब नदियों को पूर्वापर की स्मृति ही नहीं रहती, तब समुद्र कौन कहेगा? नदियों ने ही अपने लक्ष्य का नाम समुद्र रखा था। जब नाम करण वाली नदियाँ ही नहीं रहीं, तब समुद्र कौन कहेगा? जब नदियाँ नहीं, तब समुद्र नहीं। नदियों की अपेक्षा से समुद्र था। अब जो बच रहा वहाँ वह न नदी है और न समुद्र है। समुद्र को प्राप्त होने के बाद ही नदियों को मोक्ष मिलता है, नदियों के अंत होने के बाद। नदियों के अस्तित्व का अभाव अर्थात् नदियों का खतम होना ही नदियों का मोक्ष है, इसी प्रकार जीव का मोक्ष है। जीव का बंधन क्या है? जीव भाव की मान्यता ही जीव का बंधन है। आवागमन जीव का रूप है। मैं जीव हूँ-वह जीव का नाम है। मैं आत्मा को पहिले देह माना। फिर मान्यता किया कि मैं देह हूँ। यह देहाभिमान हुआ। जीव भाव के भाव में जीव का बंधन है और जीव भाव के अभाव में जीव का मोक्ष है। जीव भाव का अभाव कब और कैसे होता है? जीव भाव का अभाव आत्म भाव में होता है। आत्म भाव का भाव यह है कि मुझ आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। 'मैं हूँ', 'मैं' जैसा हूँ वैसा ही हूँ, इसका दृढ़ निश्चय ही आत्म भाव है। आज के पहिले मैं क्या था, आज क्या हूँ, कल क्या रहूँगा, आदि की तनिक भी याद न रहना तथा तीनों कालों तीनों अवस्थाओं के प्रपंचों की स्मृति का अभाव ही आत्म भाव है। जीव के मुक्त होने का वास्तविक अर्थ यही है कि जीव अपने आप से मुक्त हो जाय। भूत, वर्तमान, भविष्यत् की स्मृति का सर्वथा अभाव हो जाना ही अपने आप से मुक्त हो जाने का वास्तविक अर्थ है। यही सोइ गति है, जिसकी याचना महारानी शतरूपा ने भगवान से की।
फिर कौन सी गति? वह गति पाने के बाद पाना कुछ बाकी न रहे, जिसे प्राप्त करने के बाद प्राप्त करना कुछ भी न रहे, जिसे जान कर जानना कुछ शेष न रहे, जिसे देखकर देखने का अंत हो जाय। जब सारा प्रपंच मुझ आत्मा ही का रूप है, तब जो (प्रपंच) दिखता है, वह देखने वाला ही दिखता है, क्योंकि दिखने वाले का तो अस्तित्व ही नहीं। जब दिखना नहीं, तब देखने वाला भी नहीं है। । अत: जिस देश में दिखना और देखना दोनों का अभाव हो, वही गति।
परात्पर भाव 'मैं' आत्मा का स्वभाव जानना है। वह बिना उपकरण के जानता है। जिस तरह आँख बिना उपकरण के देखती है, कान बिना उपकरण के सुनता है, नाक बिना उपकरण के अनुभव सूँघती है। जिह्वा बिना उपकरण के रसों का स्वाद लेती है, त्वचा बिना उपकरण के अनुभव करती है। उसी तरह मैं आत्मा बिना उपकरण के जानता हूँ। यदि वास्तव में इन्द्रियों का अस्तित्व हो तो उन्हें अपने विषयों का विषय करने के लिए उपकरण की आवश्यकता हो। परन्तु, ऐसा है नहीं। इससे रपर होता है कि इन्द्रिय, इन्द्रिय नहीं है, वह परात्पर भाव 'मैं' आत्मा है। बिना उपकरण के देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि की सामर्थ्य इन्द्रियों में नहीं है, वह सामर्थ मुझ भगवान आत्मा की है। अगर आत्मा के धर्म में और इन्द्रियों के धर्म में विषमता हो, तब तो ये दो पृथक-पृथक हैं। क्योंकि दोनों के धर्म समान हैं, इसलिए इन्द्रिया का अस्तित्व भिन्न नहीं है, वे भगवान आत्मा ही हैं। जिस तरह भगवान आत्मा रामः सारा प्रपंच विकल्प है, उसी तरह मुझ आत्मा में इन्द्रियाँ अध्यस्थ हैं। जिस तरह दे को ढूँढ़ने से देह नहीं मिलती, उसी तरह इन्द्रियों को ढूँढने से इन्द्रियाँ नहीं मिलती जिस प्रकार 'मैं' आत्मा के अज्ञानी जीवों को 'मैं' आत्मा देह दिखता हूँ, उसी प्रकार अज्ञान के कारण 'मैं' आत्मा ही उन्हें इन्द्रियाँ प्रतीत होता हूँ।
देह, इन्द्रियाँ, मन आदि सब मुझ आत्मा पर अज्ञानियों के विकल्प हैं। जबः मैं देखता हूँ तब आँख देखती हैं, जब मैं सुनता हूँ तब कान सुनता है। यही बात सभी इन्द्रियों में लागू होती है। इससे सिद्ध होता है कि न तो इन्द्रियाँ हैं और न उनके धर्म हैं। जो कुछ है सब भगवान आत्मा मैं है और सब मेरा ही धर्म है। परात्पर भाव ''मैं'' आत्मा का धर्म जानना है। इसे जानकर जानना कुछ बाकी नहीं रह जाता, इसे प्राप्त कर और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इसी गति की याचना महारानी ने की ।
3. सोइ भगति -
कैसी भक्ति? सहज भक्ति ऐसी सहज भक्ति जिसके लिए कोई साधन न करना पड़े। सहज रूप में भगवान की ही भक्ति होती है, दूसरे की नहीं क्योंकि भगवान सहज है और सहज ही प्राप्त होता है। (सहज माने स्वभावत:) भगवान आत्मा स्वभावतः भगवान है। भगवान आत्मा स्व का भाव है। भगवान आ सहज है, उसकी भक्ति सहज है, उसकी प्राप्ति सहज है, उसका चिंतन सहज उसका ध्यान सहज है, उसकी धारणा सहज है अर्थात् उसका सब कुछ सहज सहज की ही भक्ति सहज होती है। जिस भक्ति में देश, काल, वस्तु की अपेक्षा नर उसको ही सहज भक्ति कहते हैं। जिस भक्ति में मन, वचन, कर्म के निरोध अथवा अनिरोध की अपेक्षा न हो, वही सहज भक्ति है। जिस भक्ति में भक्त और भगवान की स्मृति न हो, उसे सहज भक्ति कहते हैं। जिस भक्ति में अरे न हो, अटक या खटक न हो, विधि या निषेध न हो, उसे सहज भक्ति कहते हैं। महारानी शतरूपा याचना करती हैं कि हे प्रभो! आप हमें कृपा कर ऐसी ही सहज भक्ति दें।
भगवान आत्मा जो सहज है, उसे देश, काल, वस्तु आदि किसी की अपेक्षा नहीं। जो सहज है, वही सर्वत्र सदा लबालब भरा है। 'मैं' आत्मा सर्वदेश करके पूर्ण, सर्व वस्तु करके पूर्ण, पूर्ण करके पूर्ण, अपूर्ण करके पूर्ण, सर्व करके पूर्ण है। वह सर्व में है, सर्वत्र है, सर्वाधार है, सब कुछ है। भगवान् सहज होने के नाते उसकी भक्ति पूर्ण है और सहज है, इतनी सहज है कि कहा नहीं जा सकता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं- हे अर्जुन! सर्वकाल में भगवान का स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। यदि भगवान की भक्ति सहज न हो, सरल न हो, सर्वकालीन न हो, तो स्मरण भी करना और युद्ध भी करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इससे सिद्ध होता है कि इस स्मरण का संबंध मन, बुद्धि, चित्त से नहीं है। यह रमरण सर्व में हो सकता है इसलिए कि भगवान वैकल्पिक नहीं है। वैकल्पिक पदार्थ के स्मरण के लिए देश, काल, वस्तु की अपेक्षा होती है, विकल्पाधार के लिए नहीं। 'मैं' आत्मा सर्व विकल्पों का आधार हूँ, इसलिए मुझ आत्मा का चिंतन, स्मरण सब काल में हो सकता है और होता है। मैं आत्मा कहाँ नहीं हूँ, किसमें नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ? जब में आत्मा सहज हूँ, सर्वत्र हूँ, सर्व का सर्व हूँ, तो मुझ भगवान आत्मा की भक्ति भी सहज है और वह सर्वत्र सब काल में हो सकती है। मन, वाणी का विषय वैकल्पिक है और मैं भगवान आत्मा, मन, वाणी का विषय नहीं है। वह अवांग मनस गोचर है, सहज है। जहाँ मन, वाणी का व्यापार बंद हो जाता है, वही भगवान की सहज भक्ति होती है। इसलिए, उस भगवान आत्मा का स्मरण सर्वकाल में हो सकता है।
मन को रोकने के लिए कुछ करना निरोध है और कुछ न करना अनिरोध है। जिस भक्ति में मन, वचन, कर्म से कुछ न करना पड़े वही सहज भक्ति है। मन जब रूक जाता है तब क्या 'मैं' भी रुक जाता हूँ? नहीं, मैं नहीं रुकता। मन के रूकने को कौन जानता है? उसे मैं जानता हूँ। यदि मन रुकता है तो मुझे लाभ नहीं और नहीं रुकता तो मुझे कोई हानि नहीं। मैं आत्मा वहीं का वहीं रहता हूँ। इसलिए मुझ आत्मा की भक्ति के लिए मन, वचन, कर्म के निरोध अथवा अनिरोध का कोई प्रयोजन नहीं। यही मुझ आत्मा की सहज भक्ति है।
जिस भक्ति में भक्त और भगवान की स्मृति न हो, उसे सहज भक्ति कहते हैं। जब परवाना शमा में जल गया, तब परवाना के जल जाने पर शमा ही कहाँ रहा? जब नदी का अस्तित्व ही खतम हो गया, तब समुद्र ही कहाँ रहा? उसी तरह जब जीव ही नहीं रहा, जीव भाव नहीं रहा, तब ईश्वर ही कहाँ रहा? वैकल्पिक भगवान में यह बात नहीं होती।
ईसाई में गो ईसाई सा है, पर ईसाईपने की खबर ही नहीं।
इस्लाम में वो इस्लाम सा है, मगर मुस्लिमपने का असर ही नहीं।
हाँ हिन्दू में हिन्दू सा दीख पड़े, पर हिन्दूपने का बसर ही नहीं।
हर जाति में जाति उसी की है, पर जाति की उसको खबर ही नहीं।
वैकल्पिक भगवान मुस्लिमों का, ईसाइयों का, हिन्दुओं का यानि सब मजहब वालों तथा कट्टरपंथियों का होता है। हिन्दुओं का वैकल्पिक भगवान कैसा होता है? वह चोटी वाला है, मालाधारी है, चार भुजा वाला है, धनुषधारी है, मुरली वाला है। इत्यादि। संतों का, फकीरों का भगवान, भगवान है और अन्य लोगों का भगवान वैकल्पिक है। वैकल्पिक भगवान के कारण ही झगड़ा-लड़ाई व खून-खराबा होता है।
जिस भक्ति में अरे न हो वह सहज भक्ति है। अपने स्व-स्वरूप भगवान आला की भक्ति ही ऐसी है, जिसमें अरे की गुंजाइश नहीं। वैकल्पिक भगवान की भक्ति में अरे रहती है। उसमें ऐसा करो, वैसा न करो, इस वक्त करो, उस वक्त न करो, इस प्रकार करो, उस प्रकार न करो, यहाँ करो, वहाँ न करो आदि अटक रहती है। जिस भक्ति में अटक है उसमें खटक है, जहाँ खटक है वहाँ भटक है, जहाँ भटक है वहाँ लटक है, पतन है, आवागमन है। सहज भक्ति में विधि-निषेध की गुंजाइश नहीं -
विधि निषेध श्रुति शास्त्र की, मेड़ देत सब मेट।
नारायण जाके हृदय, जागत प्रेम चपेट ।।
अपने स्व-स्वरूप में निमग्न हो जाना ही भगवान की सहज भक्ति है। जीव भाद के अभाव में ही ऐसी सहज भक्ति होती है। कुछ भी न करना, कुछ भी अटक न रहन कृपा का फल है। सहज भक्ति अन-अभ्यास का फल है और अन-अभ्यास आत्म- समर्पण का पर्याय है। अभ्यास व्यक्तित्व का प्रतीक है और अपने आप 'मैं' को कुछ मानना ही व्यक्तित्व है। अपने आप 'मैं' को कुछ न मानकर शुद्ध सनातन ब्रह्म सत् चित्, आनंद जानना ही सहज भक्ति है, कृत-कृत्य पद है। इसमें न भक्त न भगवान न दृष्टा न दृश्य, न जीव न ईश्वर, न ज्ञाता न ज्ञेय, कुछ भी नहीं रह जाता। केवल मात्र 'मैं ही मैं' शेष रह जाता है।
भक्ति के विवेचन में विनय पत्रिका का निम्न पद पूर्ण रूपेण लागू होता है -
रघुपति भगति करत कठिनाई ।
कहत सुगम करनी अपार जानै सोइ जेहि बनि आई ।।1।।
जो जेहि कला कुसल ताकहँ सोइ सुलभ सदा सुखकारी।
सफरी सनमुख जल-प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी ।।2।।
ज्यों सर्करा मिलै सिकता महँ, बलतें न कोउ बिलगावै ।
अति रसग्य सूच्छम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावै ||3||
सकल दृश्य निज उदर मेलि, सोवै निद्रा तजि जोगी ।
सोइ हरिपद अनुभवै परम सुख, अतिसय द्वैत बियोगी ।।4।।
सोक मोह भय हरष दिवस निसि, देस काल तहें नाहीं ।
तुलसिदास यहि दसाहीन संसय निरमूल न जाहीं ।।5।।
जहाँ तक वाणी का विषय है सब ही दृश्य है। उसे अपने स्वरूप में मिलावे अर्थात् अपना स्वरुप आत्मा जानै। "सिया राम मय सब जग जानी", "वासुदेव सर्वमति'"। जहाँ तक मन वाणी का विषय है सब विकल्प है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच महाभूत, सब प्रपंच मात्र, मुझ भगवान आत्मा के बिना किस पर आधारित होंगे? मैं आत्मा ही सब विकल्पों का आधार हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न प्रपंच है ही नहीं। इसलिए मैं आत्मा ही सब प्रपंच हूँ। मुझ आत्मा करके ही प्रपंच की सिद्धि होती है। 'मैं' ही सब कुछ हूँ। मुझ भगवान आत्मा में सब का मिलना होता है। 'मैं' आत्मा से भिन्न कुछ रहा ही नहीं। यही हुआ सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवै निद्रा तजि जोगी। यहाँ पर सोने का अर्थ है स्थित होना। विकल्पों के अभाव में निर्विकल्पता आ जाती है। इसी निर्विकल्प अवस्था में स्थित होना है। कैसे? निद्रा तजि-मोह निद्रा तजि-यानि मुझ आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं इस निश्चय में। मुझ आत्मा से भिन्न अर्थात् मुझ आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इस अनुभूति में, इस निर्विकल्प अवस्था में स्थित होना ही परम सुख है, आत्म पद है, कैवल्य पद है, सहजानन्द है, सहज भक्ति है।
जिस समय मनुष्य गाढी निद्रा में रहता है, तब प्रपंच का अभाव रहता है, परन्तु निद्रा अर्थात् स्वप्नावस्था में प्रपंच का उदय होता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था का प्रपंच स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार जागृत अवस्था के प्रपंच का दृष्टा जागृत के प्रपंच से भिन्न नहीं होता। दोनों एक हैं। सजातीय से सजातीय का मेल होता है। सजातीय से विजातीय का मेल नहीं होता। यदि प्रपंच का स्वरूप और हो और दृष्टा यानि 'मैं' आत्मा का स्वरूप कुछ और हो तो दोनों का मेल नहीं होगा। परंतु प्रपंच और प्रपंच दृष्टा 'मैं' आत्मा सजातीय हैं इसलिए इन दोनों का मेल होता है। यदि प्रपंच मुझ आत्मा से सर्वथा भिन्न होता, तब तो प्रपंच और मैं आत्मा का मेल कभी नहीं होता। परन्तु, दोनों अभिन्न हैं, अतः 'मैं' आत्मा ही प्रपंच हूँ। इस अनुभूति में 'मैं' आत्मा के अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं और यही हरि पद है, यही परम पद है और यही सहज भक्ति है।
जब महात्मा कागभुशुंडी भगवान राम की बाल लीला देखने अयोध्या गये थे तब लीला देखते-देखते वे एकदम ऐसे भ्रम में पड़ गये कि यदि ये सच्चिदानंद भगवान हैं तो फिर इनकी यह लीला साधारण बालकों के समान कैसी? भुशुंडी जी चक्कर पड़ गये, जिसे देखकर भगवान हँस दिये। भगवान के हँसते ही भुशुंडीजी उनके पर में समा गये और वहाँ दो घड़ी में सब लीला देख लिये, परन्तु राम को एक ही देखा लीला देखकर जब महात्मा भुशुंडी बाहर आये तब भगवान प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को बोले। महात्मा कागभुशुंडि वर मांगते हैं -
अबिरल भगति विसुद्ध तव, श्रुति पुरान जेहि गाव ।
जेहि खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ।।
हे प्रभु! मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आपकी अविरल भक्ति ही चाहिए। (अविरलः अ+विरल । अ = नहीं और विरल माने जिससे भिन्न कोई दूसरा, इस तरह अविरल क अर्थ हुआ भगवान आत्मा) जिस भक्ति का गायन वेद, पुराण आदि करते हैं, संत- महात्मा गण जिसका निरूपण करते हैं, बड़े-बड़े योगी मुनि जिसके लिए याचन करते हैं, परन्तु जिसे आपकी कृपा से कोई-कोई ही पाते हैं, वही आपकी विशुर भक्ति (विशुद्ध यानि विशेष करके शुद्ध अर्थात् सब विकारों से रहित) जो सब विकार से रहित हो, मुझे कृपा करके दीजिये। अविरल तो स्वयं भगवान आत्मा ही है औ वह भगवान नहीं जिससे भिन्न कोई दूसरा हो। भगवान एक है। वह एक नहीं जिस भिन्न दो या दस, सौ या हजार या लाख आदि कुछ हो। एक के बिना किसी की सिई नहीं। एक ही सबका आधार है और वह स्वतंत्र सत्तावान है। अपना स्वतंत्र अस्तित रखने के लिए एक को किसी की अपेक्षा नहीं। इसलिए एक भगवान है। जब अविरु भगवान आत्मा 'मैं' दूसरा होता तो उसका ज्ञान बड़ा या छोटा होता, परन्तु ऐसा नहीं। जो ज्ञान, जो जाननापना, जो सतपना एक शरीर में है, वही आत्मा, वह ज्ञान, वही जाननापना सब शरीरों में है। जैसा जहाँ और जो मैं आत्मा इस शरीर हूँ, वैसा वहाँ और वही में आत्मा सर्व शरीरों में हूँ। जैसा जिसको, जिस प्रकार आत्मा इस शरीर को जानता हूँ, वैसा उसको उसी प्रकार 'मैं' आत्मा सब शरीरों सब शरीरों में जानता हूँ। इसलिए 'मैं' आत्मा अविरल हूँ और उसकी भक्ति भी अविरल है। महारानी शतरूपा ने इसी अविरल भक्ति, आत्म पद, परम पद, कैवल्य पद, कृत-कृत्य पद के लिए याचना की है।
'मैं' आत्मा सबको सब जगह से, सब काल में, सब अवस्थाओं में जानता हूँ। न शरीर अनेक हैं और न 'मैं' अनेक हूँ। 'मैं' के बिना शरीर नहीं इसलिए शरीर अनेक नहीं। 'मैं' के बिना जब शरीर नहीं, तब मैं अनेक नहीं। यदि विकल्पाधार मैं आत्मा न होऊँ, तो मान्यता किस पर मानी जायेगी? इसलिए 'मैं' ही विकल्पाधार हूँ और 'मैं' ही विकल्पक हूँ। 'मैं' आत्मा एक हूँ, इसके बोध में अन्य का अस्तित्व ही नहीं, अन्य की प्रतीति ही नहीं। इसी भक्ति को श्रुति पुराण भी गाते हैं और इसी की याचना बडे- बडे योगेश्वर तथा मुनीश्वर भी करते हैं। ऐसी अविरल भक्ति को 'मैं' ही सिद्ध करता हूँ। 'मैं' आत्मा ने ही माना और मुझ आत्मा को ही माना सारा करिश्मा 'मैं' आत्मा का ही है। यही अविरल भक्ति है और इसी विशुद्ध अविरल भक्ति की याचना महारानी ने की।
इसी अविरल भक्ति को या सहज भक्ति को पाकर भक्तगण वर्णाश्रम के अभिमान को त्याग कर दायरे से बाहर कर इस धराधाम पर स्वतंत्र होकर विचरते हैं -
चले हरषि तजि नगर नृप, तापस वनिक भिखारि ।
जिमि हरि भगति पाइ श्रम, तजहि आश्रमी चारि ।।
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में राजा, तपस्वी, बंजारा और भिखारी वृन्द एक स्थान पर रुक जाते हैं और वर्षा के अंत होते ही शरद ऋतु के आने पर अपना-अपना स्थान छोड़कर चल पडते हैं, उसी तरह शरद ऋतु रूपी विशुद्ध हरि भक्ति को पाकर भक्तगण वर्णाश्रम के अभिमान को त्याग कर अर्थात् वर्ण और आश्रम के बंधन को तोड़कर इस पृथ्वी पर स्वतंत्र होकर विचरते हैं। मनुष्य जिस भक्ति को पाकर वर्ण और आश्रम के दायरे से बाहर निकलकर पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विचरते हैं, उसको ही सहज भक्ति, सहज पद, कृतकृत्य पद कहते हैं। जब तक वर्णाश्रम का अभिमान है, तब तक देहाभिमान है। देहाभिमान देहाध्यास पर आधारित रहता है और देहाध्यास स्वरूप के अज्ञान से होता है। देहाध्यास के छूटने पर देहाभिमान अर्थात् मैं देह हूँ, यह देह मेरा है, इस प्रकार की धारणा का त्याग हो जाता है और देहाभिमान के अभाव में वर्ण और आश्रम का भी अभिमान गल जाता है। जब वर्णाश्रम का अभिमान गल जाता है, जब अपने आप को शुद्ध आत्मा 'मैं' का 'मैं' अनुभव करने लगता है, तब वह भक्त कर्म के बंधनों से बाहर निकल जाता है और श्रुतियों के बताये मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं रहता। ऐसी अनुभूति ही हरि भक्ति है, सहज भक्ति है, अविरल भक्ति है और महारानी शतरूपा ने इसी के लिए याचना की है। यही है "सकल दृश्य निज उदर मेलि निद्रा तजि सोवै जोगी।"
इस संसार में अज्ञान रूपी रात्रि में परमार्थी-जिसकी दृष्टि में मुझ आत्मा से भित्र कुछ है ही नहीं-और प्रपंच वियोगी ही यानि जिस की दृष्टि में प्रपंच नाम की कोई चीज ही नहीं, जागते हैं। "एहि जग जामिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच बियोगी।" और "जानिअ तबहिं जीव जागा। जब सब विषय बिलास बिरागा।" अनादि काल की अविद्या की निद्रा से जब जीव जागता है, तब वह अनुभव करता है कि मुझ आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। उसे अनुभूति होती है कि न प्रपंच है, न इन्द्रियाँ है, न देह है, न और कुछ है, सब कुछ 'मैं' ही 'मैं' हूँ। परन्तु, जब मोह निशा में सोता है, तब कहता है कि मैं संसारी जीव हूँ, मैं जन्मता-मरता हूँ, मैं आता - जाता हूँ, मैं स्वर्गी-नर्की हूँ आदि। मोह निशा से जागने पर अपने आप मैं आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता। उसकी दृष्टि में हर्ष-शोक, सुख-दुःख, देश-काल, हानि- लाभ आदि कुछ भी नहीं रहता, वह केवल 'मैं' का ही अनुभव करता है। उसकी निर्विकल्प अवस्था हो जाती है और यही निर्विकल्पानुभूति ही सहज भक्ति है, परम सुख है, आत्मानंद है और इसी के लिए महारानी ने याचना की।
जब तक हरि भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, तब तक संशय विपर्यय का नाश नहीं होता। स्वरूप का बोध होने पर ही संशय-विपर्यय, मद, माया आदि का नाश होता है। कहा गया है -
बिमल ग्यान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई ।।
सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ।।
विमल ज्ञान माने आत्म अनुभव, स्वरूप का बोध। स्वरूपानंद रूपी जल मे डुबकी लगाना ही रामभक्ति में सराबोर होना है। उस आत्मानुभूति के फलस्वरूप आत्मज्ञानी का माया का बंधन (माया अर्थात् मान्यता अपने आप 'मैं' आत्मा को देह मानना) तथा उसका मद अर्थात् अभिमान, देहाभिमान (यह देह मैं हूँ, यह देह मेरा है आदि) नाश हो जाता है। राम की भक्ति में सराबोर भक्त, अपने स्वरूपानंद में सर्वदा निमग्न रहने वाला तत्त्व ज्ञानी न तो कभी माया के चक्कर में फँसता है और न कभी देहाभिमान होता है। उसकी दृष्टि में सिवाय एक भगवान आत्मा 'मैं' के कुछ भी नहीं रहता। यही स्वतंत्र भक्ति है। इसी स्वतंत्र भक्ति या सहज भक्ति के अधीन ज्ञान- विज्ञान सभी रहते हैं और महारानी शतरूपा ने इसी की याचना भगवान से की। यह भक्ति न परा है, न अपरा है, न सगुण ब्रह्म की है और न निर्गुण ब्रह्म की। यह भगवान की भक्ति है, स्वतंत्र और सहज। यह भगवत् कृपा अर्थात् संत कृपा से प्राप्त होती है। यह साधन साध्य नहीं है, केवल कृपा साध्य है।
4. चौथा वर जो महारानी शतरूपा ने भगवान से मांगा वह भगवान के श्रीचरणों में सहज सनेह है। सहज सनेह वह है जो बिना किसी साधन के, बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो। ऐसा सहज सनेह भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। जो भक्त हैं, वे भगवान के भक्त होते हैं। उनके लिए सगुण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। उनके लिए भगवान माने भगवान, व्यापक भगवान जो चर-अचर में, कण-कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र ठसाठस भरा है। भगवान में सगुण या निर्गुण का विकल्प भक्तों की भावना का द्योतक है और भगवान के यथार्थ स्वरूप के अज्ञान का परिणाम है। संत तुलसीदास जी ने कहीं पर भी सगुण निर्गुण, साकार या निराकार ब्रह्म में भेद नहीं माना है। जो निर्गुण है, वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है। यथा -
सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ।
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसे ।।
शंकर गीता के अंतर्गत भगवान शिव ने सच्चिदानन्द भगवान श्रीराम के स्वरूप का जो वर्णन किया है तथा विवाहोपरान्त बिदाई के समय जनक जी ने भगवान राम की जो स्तुति की है वे सगुण निर्गुण की अभेदता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ऐसा सर्व व्यापक भगवान सगुण भी है, जो निर्गुण भी है, उसके चरण कमलों में सहज सनेह की याचना महारानी शतरूपा ने की।
रामानुज भरत बोधवान थे। भगवान श्रीरामचन्द्र जी के चरण कमलों में उनका अटूट प्रेम था। फिर भी वे गंगा मैया से याचना करते हैं -
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरबान ।
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ।।
जब-जब मैं जन्म धारण करूँ भगवान श्रीराम के चरण कमलों में मेरा सहज सनेह हो, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यद्यपि बोधवान को किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, तथापि भगवान के प्रति कृतज्ञता जताने को उनके चरण कमलों में सहज सनेह के लिए प्रार्थना करते हैं। बोधवान होने पर ही भगवान के चरण कमलों में सहज सनेह होता है। जो अपने को संसारी जीव मानता है, उसका जीव हृदय कभी भी कामना रहित नहीं हो सकता। कामना रहित आत्म-देश का निवासी अर्थात् आत्म वेत्ता ही हो सकता है और ऐसे भक्तों को भगवान के चरण कमलों में सहज सनेह की ही आकांक्षा रहती है और महारानी शतरूपा ने भगवान के चरण कमलों में ऐसे ही सहज सनेह की याचना की।
भगवान राम अपने श्रीमुख से कहते हैं -
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा।
सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहिं बाँधि बरि डोरी ।।
माता-पिता, भाई, स्त्री, पुत्र परिवार, तन, धन, धाम आदि सबका माया-मोड मन से त्याग कर इनके मोह रूपी धागे को रस्सी के रूप में बटकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों में बाँध दे। तात्पर्य, यह है कि संसार का, स्वजन का तथा अन्य सबका मोह-ममता त्याग कर भगवान के चरण कमलों में निष्कपट प्रीति करे। जब तक भगवत् चरणों में अनन्य प्रेम नहीं होगा, तब तक मोह ममता आदि माया के विकारो का त्याग नहीं होगा और हृदय कामना रहित नहीं होगा। भक्तों के अनन्य प्रेम, सहज सनेह के वशीभूत होने के कारण ही अजन्मा, असंग, निर्गुण, निरंजन, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वात्मा भगवान राम को शरीर धारण कर प्रगट होना पड़ता है। भगवान फिर कहते भी हैं -
अस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदयें बसइ धनु जैसे ।
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे । धरउँ देह नहिं आन निहोरे ॥
ऐसे ही अनन्य भक्तों के सहज सनेह के समान श्री चरणों में सहज सनेह के लिए महारानी शतरूपा ने भगवान से याचना की।
5. महारानी शतरूपा ने पांचवीं वस्तु जो मांगी है सोइ विवेक ? उसका स्वरूप भगवान के श्रीमुख से -
सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक ।
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक ।।
अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तजि दोष गुनहिं मन राता ।।
भगवान श्रीरामचन्द्र जी भरत जी से कहते हैं कि माया रचित इस संसार में अनेकों गुण हैं और अनेकों दोष हैं, उनमें इतने गुण-दोष हैं कि जितनी गिनती नहीं परन्तु, गुण अर्थात् विवेक यही है कि दोनों को यानि गुण और अवगुण (दोष) कोन देखे, उनको सर्वथा त्याग देवें और यदि देखता है तो वही अविवेक है, अज्ञान है, ऐसा विवेक यानि गुण व अवगुण का त्याग तभी प्राप्त होता है जब विधाता की कृपा होती है। यह विवेक अन्य प्रकार से नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा विवेक, ऐसा सहज ज्ञान, भगवत् कृपा पर अवलम्बित है। यह कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। ऐसा विवेक जिसमें गुण और दोष दोनों न देखे जायें, दोनों का त्याग किया जाय, वह परमहंस दृष्टि, भगवत् दृष्टि कहलाता है।
दृष्टि तीन प्रकार की होती है -
1. काग दृष्टि - जिसमें गुण को त्यागकर कर दोष को ग्रहण किया जाता है।
2. हंस दृष्टि - जिसमें दोष को त्याग कर गुण ग्रहण किया जाता है।
3. परहंस दृष्टि - जिसमें गुण और दोष दोनों को त्याग कर केवल भगवान आत्मा 'मैं' को ग्रहण किया जाता है, जिसमें 'मैं' आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की प्रतीति नहीं होती।
भगवत् दृष्टि में गुण या दोष कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं रहता। जहाँ अपना आप 'मैं' आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, वहाँ माया जनित गुण-दोष कहाँ? जब अपने आप 'मैं' आत्मा को कुछ माना जाता है, तब माया के वश में होना पड़ता है और तब ही किसी में दोष और किसी में गुण दिखाई देते हैं। जब किसी को नर माना जाता है, तब उसमें गुण और दोष भी दिखता है। जब उसे नारायण जाना जाता है, तब उसमें गुण दिखते हैं और न दोष दिखते हैं। नारायण में, भगवान में गुण-दोष नहीं हैं। गुण और दोष मानने में निहित है, जानने में नहीं। गुण देखकर राग होता है और दोष देखकर विराग अथवा त्याग होता है। मानना ही अविवेक है और जानना विवेक है। यदि जानने चलो तो सब कुछ अपना आप 'मैं' भगवान आत्मा दिखेगा। सबको अपना स्वरूप जानना, अपने आप 'मैं' आत्मा को 'मैं' का 'मैं' ही जानना परमहंस दृष्टि है और यही विवेक है।
माया में गुण-दोष की प्रतीति कैसे होती है? अनादिकाल से जीव अपने आपको कुछ न कुछ मानकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। जब अपने आपको माना कि 'मैं ऐसा हूँ' तो ऐसा मानना ही माया है। इस पद में 'मैं' के अतिरिक्त दूसरे दिखाई देंगे और तब अपने अंदर और अपने बाहर भी गुण-दोष दिखाई देंगे। जो जैसा अपने आपको मानता है वैसा ही उसे अपनी परछायी सब जगह दिखाई देती है। जो अपने आपको कुछ न मानकर 'मैं' जैसा हूँ, वैसा ही हूँ-ऐसा जानता है वह भगवान है और यही विवेक है। जिसका निश्चय जैसा अपना आप 'मैं' हूँ वैसा ही हूँ-ऐसा हो तो वही गुण-दोष का त्याग है और वही परमहंस दृष्टि है। जब अपने आप 'मैं' आत्मा को जान लेता हूँ, तब संसार भी अपने 'मैं' का स्वरूप दिखाई देता है। जब संसार अपना आप मैं दिखाई देता है, तब न गुण दिखाई देता है और न दोष दिखाई देता है। अपने आप 'मैं' को बिना कुछ माने विकार (काम, क्रोध आदि) भी सामने नहीं आते। जितने भी विकार हैं सब अपने आप 'मैं' को कुछ मानने पर ही पैदा होते हैं। अपने आप मैं को 'मैं' जानने में किसी भी प्रकार के विकार का आक्रमण नहीं होता। जो अपने आप मैं को 'मैं' ही जानना है वही भगवान है और यही विवेक है।
अपने आप 'मैं' को - मैं अमुक हूँ-मानना माया है। इस अमुक भाव का आधार 'मैं' आत्मा हूँ। बिना 'मैं' के अमुक नहीं। इसलिए 'मैं' ही अमुक रूपी माया का आधार, पति, रक्षक हुआ। भगवान आत्मा को जान लेने पर ही माया से छुटकारा मिलता है। जब भगवान आत्मा को यानि 'मैं' को 'मैं' जानना ही विवेक है, तब भगवान को जानना सहज है। वैकल्पिक भगवान (भगवान ऐसा है) को जानना कठिन है, परन्तु यथार्थ भगवान को (भगवान जैसा है वैसा ही है) जानना सहज है। 'मैं' हूँ-बिना किसी मान्यता के, बिना कोई आकार-प्रकार के, इसका ज्ञान ही सहज विवेक है। विवेक का विवेक होना कृपा साध्य है। यह साधन का विषय नहीं है। 'मैं हूँ इस विवेक को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है। परन्तु, यम नियम द्वारा, मन, वचन, कर्म द्वारा जो भी साधन किये जाते हैं, वे वैकल्पिक भगवान (भगवान ऐसा है या 'मैं' ऐसा हूँ) के लिए किये जाते हैं। जो कुछ ि करना धरना है सब माया देश में है। 'मैं हूँ' इसके लिए कुछ करना धरना नहीं है। कुछ करो तब भी 'मैं' आत्मा हूँ और कुछ न करो तब भी मैं आत्मा हूँ। यह सहज विवेक सतकृपा या भगवत कृपा का फल है और इसी सहज विवेक के लिए महारानी शतरूपा ने भगवान से याचना की।
6. छठवाँ पद जिसके लिए महारानी शतरूपा की प्रार्थना थी, वह है "सोइ रहनि" कैसी रहनी? इसकी झलक विनय पत्रिका के नीचे के पद से मिलती है कि
कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगो।
श्री रघुनाथ कृपालु कृपातें', संत-सुभाव गहौंगो ।।1।।
यथा लोभ संतोष सदा, काहूसों कछु न चहौं गो ।
पर हित-निरत निरंतर, मन-क्रम-बचन नेम निबहौंगो ।।2।।
परुष बचन अति दुसह श्रवन सुनि, तेहि पावक न दहौंगो ।
बिगत मान सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोष कहौंगो ||३||
परिहरि देह जनित चिंता, दुख-सुख समबुद्धि सहौंगो ।
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अबिचल हरि भगति लहौंगो ||4||
भक्त अपने भगवान से प्रार्थना करता है, हे दयानिधान श्री रघुनाथजी! आपकी कृपा से मुझे संतों का सा स्वाभाव कब मिलेगा? जब आपकी कृपा होगी तब ही मुझे संतों का सा स्वभाव और संतों के समान रहन-सहन मिलेगा। जो कुछ भी सरलतापूर्वक प्राप्त हो उस पर ही संतुष्ट रहना, किसी से कुछ भी वस्तु की मांग न करना और न किसी वस्तु की कामना करना, सदा ही मन, वचन, कर्म से दूसरों की भलाई करने में लगे रहना, किसी का भी कठोर वचन सुनकर क्रोधित न होना तथा उसे शांतिपूर्वक सुन व सह लेना, कभी भी अपमान की आग में न जलना, सब प्रकार की मान्यताओं को त्याग कर समदर्शी होकर विचरना तथा किसी के गुण अथवा दोष को न देखना, देह जनित सारी चिंताओं को त्याग देना, सुख-दुःख को बराबर मानकर समबुद्धि से निर्वाह करना, इस प्रकार का स्वभाव और ऐसी संत रहनी मुझे प्राप्त हो। ये सब बातें साधन साध्य न होकर भगवान की कृपा पर अवलंबित हैं। जब भगवान की कृपा होगी तब ही इस प्रकार की मनोवृत्ति बनेगी और इस प्रकार की रहनी मिलेगी और तब ही भगवान के चरणों में अविरल भक्ति होगी। महारानी शतरूपा ने इसी संत रहनी के लिए भगवान से प्रार्थना की।
'सोइ रहनि' याने संत रहनी। इसका दूसरा भाव सहजावस्था है। जब 'मैं हूँ' - इसका ज्ञान सहज है तो इसकी रहनी भी सहज है। यद्यपि मैं हूँ - इसका ज्ञान सबको है, फिर भी मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। में कैसा हूँ, मैं क्या हूँ आदि प्रकार के प्रश्न जहाँ उठे कि वहाँ मान्यता आ गयी और सहजपना जाता रहा। कुर्सी है नहीं, मेज है नहीं, परन्तु दिखाई दे रहे हैं। यथार्थ में लकड़ी दिखाई दे रही है। संसार है नहीं, परन्तु दृष्टिगोचर हो रहा है। वस्तुतः, वह भगवान है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब भगवान है। फिर ऐसा क्यों भान नहीं होता कि मैं भगवान देख रहा हूँ? जब में स्वतः भगवान हूँ तो फिर कैसे भान होगा कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वह सब भगवान देख रहा हूँ और भगवान के सिवाय कोई दूसरा देखने वाला हो, तो उसे भान हो कि 'मैं' भगवान देख रहा हूँ। जब में देखने वाला ही भगवान हूँ और जिसको देखता हूँ वह भी भगवान ही है, तो फिर भगवान देखने का भान किसको होगा और कैसे होगा? भान तो दो में होता है। जब मैं ही 'मैं' हैं, जब मुझसे भिन्न कोई दूसरा नहीं तो फिर किसको भान हो कि मैं भगवान देख रहा है। सबको देखने वाले को, सबको जानने वाले को कौन दूसरा देखेगा, कौन दूसरा जानेगा जब कोई दूसरा 'मैं' आत्मा के अतिरिक्त है ही नहीं? यही निश्चय ही, इसी स्थिति में स्थित होना ही सहज रहनी है, सहजावस्था है। जब अपने आप 'मैं' को कुछ माना, तब क्या बिगड़ा और जब जाना तब क्या बना? कुछ बिगड़ा और रन कुछ बना। मैं जैसे पहिले था वैसे अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मुझ आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं।
यही निश्चय ही, इसी पर निष्ठा ही सहज रहनी है, सहजावस्था है और इसी की प्राप्ति के लिए महारानी शतरूपा ने भगवान से कृपा कर देने की प्रार्थना की ।। 151||
सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना । कृपासिंधु बोले मृदु बचना ||1||
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ।।2।।
मातु बिबेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ||३||
कोमल, गूढ़, सुन्दर और श्रेष्ठ प्रार्थना (रचना) को सुनकर दयासागर प्रभु कोमल वचन बोले कि तुम्हारे मन में जो कुछ है, तुम्हारी जैसी रुचि है, वह सब मैंने तुम्हें दी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हे माता! मेरी कृपा से तुम्हारा यह अलौकिक ज्ञान कभी नहीं मिटेगा।
भगवान ने दम्पति के इस संदेह को कि सारे चराचर के स्वामी जगत् के आधार ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के उत्पत्ति कर्ता प्रभु हमारे पुत्र होंगे कि नहीं, महारानी शतरूपा को माता का संबोधन देकर यहीं पर निर्मूल कर दिया और भगवान ने माता के विवेक को अलौकिक इसलिए कहा कि बहुधा पुत्र पर माता-पिता का प्यार अंघ होता है, परन्तु माता कौशल्या का प्यार भगवान श्री रामचन्द्र जी पर असीम और मातृवत् होते हुए भी एक उच्च कोटि के भक्त का सहज सनेह था। भगवान की लील देखते हुए माता जी कई भ्रम में पड़ गई थी, परन्तु प्रभु की कृपा से तुरन्त ही संभल जाती थी और भक्त विषयक ज्ञान जागृत हो जाता था। अतः, अलौकिक विवेक प लोकोत्तर ज्ञान कहा है।
बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी । अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥
सुत विषइक तव पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ ॥
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना । मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥
चरणों में प्रणाम करके मनु महाराज फिर बोले हे प्रभो! मेरी और भी एक प्रार्थना है। चाहे कोई मुझे मूर्ख या मंद बुद्धि क्यों न कहे, आपके चरण कमलों में मेरी प्रीति पुत्र भाव से हो। जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे। तात्पर्य है कि जैसे जल से बिलग होते ही मछली मर जाती है, वैसे ही आपके बिछडुते ही मेरे जीवन का भी अंत हो जाये।
अस बरु मागि चरन गहि रहेउ । एवमस्तु करुणानिधि कहेऊ ॥
अब तुम मम अनुसासन मानी। बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥
ऐसा वर मांग कर वे भगवान के चरणों को पकड़कर रह गये। तब दयानिधान प्रभु ने एवमस्तु (ऐसा ही हो) कहा औरफिर बोले कि अब तुम मेरी आज्ञा मानकर स्वर्ग लोक में जाकर निवास करो।
सोरठा - तहँ करि भोग बिलास, तात गएँ कछु काल पुनि ।
होइहहु अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत ।।152||
हे तात! वहाँ भोग विलास करते हुए कुछ समय तक रहो, उसके बाद जब तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा।
इच्छामय नर वेष सँवारे । होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे ।।
अंसन्ह सहित देह घरि ताता। करिहउँ चरित भगत सुखदाता ॥
हे तात! अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण करके अपने अंशों के सहित तुम्हारे घर में प्रकट होऊँगा और भक्तों को सुख देने वाले अनेकों चरित्र करूंगा।
भगवान यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि जो रूप अभी तुम देख रहे हो उस रूप से न आकर अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण कर भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तथा उनको कुछ देने के लिए अकेले न आकर अपने अंशों के साथ अनेकों प्रकार की नर लीला करने प्रकट होऊँगा। भगवान अजन्मा होने के नाते जन्म धारण नहीं करते। उनका शरीर रज, बीर्य जनित पाँच भौतिक न होकर चिदानन्दमय होता है और इच्छामय होता है अर्थात् लोगों को उनकी अपनी भावनाओं के अनुरूप दिखाई देता है।
भगवान अंशों के सहित प्रकट होने का वचन दे रहे हैं। वे अंश कौन-कौन से हैं जो परात्पर प्रभु के साथ इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए? 'नारद पंचरात्र' में बैकुण्ठाधीश श्रीविष्णु का भरत रूप में, शेषशायी श्रीमन्नारायण का लक्ष्मण रूप में और श्वेत द्वीप निवासी भूमापुरुष का शत्रुघ्न रूप में श्रीराम सेवार्थ अवतीर्ण होने का उल्लेख है। इसकी पुष्टि नामकरण के समय गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा भी हो जाती है। विष्णु जगत् का पालन भी करते हैं, अतः "विश्व भरन-पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई।" शेषशायी श्रीमन्नारायण इस जगत् के आधार तथा धरा के धारण करने वाले हैं। अतः, लक्ष्मण जी शेषाशायी श्रीमन्नारायण हैं। भगवान की स्तुति करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण जी के संबंध में व्यक्त किया है- 'जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी ।' जो हजार सिर वाले शेषनाग के स्वामी श्रीमन्नारयण हैं, जो इस धराधाम को धारण किये हुए हैं, वे लक्ष्मण जी के रूप में प्रगट हैं और शत्रुघ्न के रूप में भूमापुरुष के लिए कहा है-"जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम सत्रुहन बेद प्रकासा ॥" स्मरण करने से भूमापुरुष भगवान राम, शत्रुघ्न के रूप में भक्तों के दुःख व विकार रूपी शत्रुओं का नाश करते हैं। इस प्रकार ये तीनों जो परात्पर पुरुष भगवान श्रीराम के अंश हैं, श्रीरामचन्द्र जी के भाई के रूप में अवतीर्ण हुए।
जे सुनि सादर नर बड़ भागी। भव तरिहहिं ममता मद त्यागी ।।
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥
जो बड़े भाग्यशाली मनुष्य मेरे उस भगवत् चरित्र को आदरपूर्वक तथा मोह ममता और (मद) देहाभिमान को त्यागकर सुनेंगे, वे संसार सागर को सरलतापूर्वक तर जायेंगे। मेरी आदिशक्ति, मेरी परमाशक्ति प्रकृति स्वरूपा माया, ये भगवती सीता जी भी, जो अखिल ब्रह्माण्ड का सृजन करती हैं, पृथ्वी पर अवतार लेंगी। (यही त्रिगुणात्मिका माया यानि सीताजी, जो संसार की उत्पत्ति कत्री हैं, भगवान राम के अयोध्या में जन्म लेने से लेकर राजगद्दी तक के समस्त चरित्र की है। अजन्मा अकर्त्ता भगवान राम कुछ भी नहीं किये। सारा राम-चरित्र सीता रूपिणी आदि शक्ति माया का किया हुआ है)।
पुर उब मैं अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य प्रन सत्य हमारा ।।
पुनि-पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतरधान भये भगवाना ॥
मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूँगा, मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य है, सत्य है, सत्य है। बारम्बार ऐसा कहकर दयासागर भगवान राम अदृश्य हो गये।
दम्पति उर घरि भगत कृपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काला ॥
समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति बासा ।।
वे दोनों स्त्री-पुरुष यानि महारानी शतरूपा और महाराज मनु भगवान की भक्ति को हृदय में धारण कर कुछ समय पर्यन्त उस आश्रम में और निवास किये। तत्पश्चात् समय पाकर बिना कष्ट शरीर त्यागकर इन्द्रलोक में जाकर सुख भोगने लगे ।।7, 8।।
दोहा- यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहि वृष केतु ।
भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ||153 ||
॥ इति श्री मनु शतरूपा बरदान आख्यान समाप्त ।।
द्वितीय खण्ड़
1. लक्ष्मण गीता
2. वाल्मिकी आश्रम
3. चित्रकूट दरबार
1. लक्ष्मण गीता
आत्म जिज्ञासुओं!
जिस समय भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वन यात्रा में गंगा तट पर पहुँचे तो वहाँ पर भगवान राम रात के समय सिंसुपा वृक्ष के नीचे जंगली पत्तों का बिछौना बनाकर भूमि पर सोये। भगवान राम को जमीन पर सोते देखकर, निषाद राज को बड़ा दुःख हुआ। उसका शरीर रोमांचित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा, वह प्रेम सहित लक्ष्मण से कहने लगा।
महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुन्दर है, इन्द्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुन्दर मणियों से रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाकर सजाया है। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुन्दर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगन्ध से सुवासित हैं। जहाँ, सुन्दर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। जहाँ ओढ़ने-बिछाने के अनेक दिव्य वस्त्र, तकिये और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुन्दर हैं, उन चौबारों में भगवान श्रीराम और माता सीताजी शयन करते थे। जो अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे, वही माता सीता और श्रीराम आज घास-फूस की साथरी पर थके हुए, बिना बिछौने के ही सोये हैं। ऐसी दशा में देखे नहीं जा सकते -
मातु पिता परिजन पुरबासी । सखा सुसील दास अरु दासी ।।
जोगवहिं जिन्हहि प्रान की नाई। महि सोवत तेइ राम गोसाईं ।।
पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ । ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ।।
रामचंदु पति सो बैदेही । सोवत महि बिधि बाम न केही ।।
सिय रघुबीर कि कानन जोगू । करम प्रधान सत्य कह लोगू ।।
( अ.क.-दो. 90 के बाद)
भगवान राम और सीता क्या वन के योग्य हैं? लोग कहते हैं कि विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता।
दोहा- कैकयनन्दिनी मंदमति, कठिन कुटिलपन, कीन्ह।
जेहिं रघुनंदन जानकिहि, सुख अवसर दुखु दीन्ह ।।
(अ.क.दो. 91)
निषादराज, लक्ष्मण से कहने लगा कि नीच बुद्धि कैकेई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने श्रीराम और जानकी के सुख के समय दुःख दिया।
भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी। कुमति कीन्ह सब बिस्व दुखारी ।।
वह सूर्य कुलरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गयी। उस कुबुद्धि ने सम्पूर्ण विश्व को दुःखी कर दिया।
भयउ विषादु निषादहि भारी। राम सीय महि सयन निहारी ।।
भगवान राम और माता सीता की इस दशा से दुःखी निषाद जब बार-बार कैकेई पर दोष लगाने लगा तब लक्ष्मण बड़े प्रेम से उसे शान्त करने के लिए कोमल वचनों से ज्ञान, वैराग्य और भक्तिरस से सनी हुई वाणी कहने लगे। लक्ष्मण का निषाद के प्रति यह जो उपदेश हुआ, उसे सन्त समाज में 'लक्ष्मण गीता' कहते हैं।
बोले लखन मधुर मृदु बानी। ग्यान बिराग भगति रस सानी ।।
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सबु भ्राता ।।
भाई निषाद इस संसार में कोई किसी को सुख-दुःख देने वाला नहीं है। सब अपने-अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। इसलिए कैकेई माता पर दोष लगाना ठीक नहीं। इसी आशय पर गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत से कहा था कि -
दोहा - सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ ।
हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ।।
(अ.का. 171)
गुरुदेव वशिष्ठ शोक भरे शब्दों में भरत से कहते हैं कि भैय्या भरत ! भावी बड़ी प्रबल होती है, यह विलखि अर्थात् लखने की चीज नहीं है, क्या किसी ने अपने भावी अर्थात् प्रारब्ध को देखा है? इसलिए, हानि-लाभ, जीवन-मरण, सुख-दुःख, यश- अपयश की जो विधि (तरीका) है, वह अपने हाथ में है।
पुण्य-पाप बान्ध्यो जगत, को काटै समरथ्थ ।
ऐसे ज्ञानिन के कहे, यह सब अपने हथ्थ ।।
भूतकाल अर्थात् अतीत के पुरुषार्थ को संचित कहते हैं। उसी संचित के कुछ हिस्से को 'प्रारब्ध' कहते हैं और वर्तमान के पुरुषार्थ को 'क्रियमाण' कहते के कुछ देश में प्रारब्ध प्रधान है और आत्मदेश में पुरुषार्थ प्रधान है।
'काहु न कोऊ दुःख-सुख कर दाता' से ज्ञान का प्रसंग शुरू होता है और प्रारब्ध भोग अज्ञान के अंदर है। 'निज कृत कर्म भोग सब भ्राता' यह तो पुरुषार्थ का फल हुआ और सुख-दुःख कर्म का फल है।
जोग बियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ।।
जनमु मरनु जहँ लगि जग जालू। संपति बिपति करमु अरु कालू ।।
धरनि धामु धनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जहुँ लगि व्यवहारू ।।
देखिअ सुनिअ-गुनिअ मन माँही । मोह मूल परमारथ नाहीं ॥
योग-वियोग, भोग, सम्पत्ति और विपत्ति, भला और बुरा, कर्म (संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण) और काल (भूत, भविष्यत्, वर्तमान) धरणि धन, धाम, कुटुम्ब, परिवार, स्वर्ग और नरक ये सब जहाँ तक व्यवहार में देखे, सुने और गुने जाते हैं, कहाँ है? तो मानसकार कहते हैं कि देखना, सुनना और गुनना ये सब 'मनमाँही' है। मन में है, बाहर नहीं, और मन कहाँ है? तो मन अज्ञान से पैदा होता है 'मोह मूल' अर्थात् मन का मूल कारण अज्ञान है। परमार्थ अर्थात् स्वरूप आत्मा में इसका सर्वथा अभाव है। विषय समझो - गाढ़ी नींद, सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं रहता, क्योंकि वह अपने कारण अज्ञान में लीन रहता है। मन के लीन होने के तीन स्थान हैं- सुषुप्ति, मूर्च्छा और समाधि।
सुषुप्ति में मन अज्ञान में लीन होता है। मूर्च्छा में मन दुःख में लीन होता है और समाधि में मन आनन्द अर्थात् स्वरूप में लीन होता है। बन्धन और मोक्ष का कारण भी मन ही है। सुषुप्ति अवस्था (गाढी नींद) में जब मन का अभाव रहता है, तब मन से उत्पन्न सारे प्रपंचों का भी अभाव रहता है, क्योंकि इन प्रपंचों का जो कारण मन है जब वही नहीं रहता, तब उसका कार्य, यह सारा प्रपंच भी नहीं रहता। मन के अभाव में "योग वियोग भोग भल मन्दा" से लेकर "मोह मूल परमारथ नाहीं" तक जितने प्रपंच हैं, वे भी नहीं रहते। मगर शुद्ध स्वरूप 'मैं' आत्मा तो रहता हूँ। मेरा अभाव नहीं होता।
देखो भैय्या ! यहाँ पर अब हम मन के विषय में कुछ कहेंगे, क्योंकि -
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ।
पार ब्रह्म को पाइये, मन ही के परतीत ।।
जिसको तुम अविद्या, अज्ञान, संसार कहते हो उसी को व्यष्टि जगत् में मन और समष्टि जगत् में माया कहते हैं। इस मन की बीमारी से कोई अछूता नहीं है। यह बीमारी सबको है। राजा, भिखारी, मूर्ख, विद्वान, गृहस्थी, विरक्त किसी को भी इस बीमारी से छुट्टी नहीं। इससे छुट्टी तो उसी को मिलती है, जिस पर सन्तकृपा हो जाती है। मानसकार विनय में कहते हैं -
जौ निज मन परिहरै बिकारा ।
तौ कत द्वैत-जनित संसृति-दुख, संसय सोक अपारा ।।
(पद 124)
द्वैत का अर्थ होता है दो। जन्म-मरण, पाप-पुण्य, शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, बन्ध-मोक्ष, ज्ञाता-ज्ञेय, द्रष्टा-दृश्य आदि ये जितने द्वैत हैं, दो हैं। सब मन के विकार हैं, यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुःख, भ्रम आदि अपार शोक क्यों हो। यह सब मन के कारण ही होता है।
सत्रु, मित्र, मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें बरिआई ।
त्यागन, गहन, उपेच्छनीय, अहि, हाटक, तृनकी नाई ॥
शत्रु, मित्र और उदासीन इन तीनों की मन ने ही हठ से कल्पना कर ली है। शत्रु को साँप के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को सुवर्ण के समान ग्रहण करना चाहिए और उदासीन की तृण के समान उपेक्षा कर देना चाहिए। ये सब मन की ही कल्पनाएँ हैं।
असन, बसन, पसु, बस्तु, बिबिध-बिधि, सब मनि महँ रह जैसे ।
सरग, नरक, चर-अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे ॥
जैसे बहुमूल्य मणि में भोजन, वस्त्र, पशु और अनेक वस्तुएँ भरी रहती हैं, उस प्रकार स्वर्ग, नरक, चर, अचर और बहुत से लोक-लोकान्तर इस मन में भरे हैं। भा यह है कि जैसे बहुमूल्य मणि को बेचकर उस मिले हुए दामों की रकमों से भोजन सामग्री, तरह-तरह के वस्त्र, पशु, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस आदि खरीद लिये जा हैं, तब ये सब मणि में हैं। इसी तरह स्वर्ग-नरक, चर-अचर और लोक-लोकान ये सब मन के भीतर हैं।
बिटप-मध्य पुतरिका, सूत महँ, कंचुकि बिनहिं बनाये ।
मन महँ तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाये ।।
किसी वृक्ष को बढ़ई को दिखा दो तो वह उसे देखकर कह देगा कि इससे इतनी कुर्सियाँ, तख्त, टेबिल, बेंच, दरवाजे, चौखट आदि बनेंगे। ऐसे ही किसी बुनकर के सामने सूत का बिन्डल अथवा गट्टा रख दीजिए, तो वह भी उससे बन सकने वाले कपड़े, चद्दर, धोती आदि की संख्याएँ बिना बताये ही बता देगा। तात्पर्य यह कि वृक्ष में टेबिल, कुर्सी, बेंच, तख्त तथा सूत में वस्त्र बिना बनाये ही भरे हैं। उसी प्रकार इस मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं, जो समय पाकर प्रगट होते रहते हैं।
देखो, कभी-कभी स्वप्न होता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। प्रश्न होता है कि मैं तो आकाश में कभी नहीं उड़ा तब ऐसा स्वप्न कैसे देखा। उत्तर है- अरे ! इस जन्म में न सही, किसी जन्म में उड़े होंगे।
रघुपति-भगति-बारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझै ।
तुलसिदास कह चिद्-बिलास जग, बूझत-बूझत बूझै ।।
जब भगवान की भक्ति रूपी जल से चित्त धुलकर निर्मल हो जायेगा तब अनायास ही स्व-स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव हो जायेगा।
श्री मानसकार कहते हैं कि जगत् भगवान आत्मा का विलास है। यह समझते - समझते ही समझा जाता है। बूझते-बूझते तीन बार बूझत-बूझत क्यों कहा गया? इसका उत्तर विनय के एक सौ ग्यारह नम्बर के पद में मिलेगा। इस पद में मानसकार कहते हैं कि इस संसार को कोई सत्य कहता है, कोई असत्य कहता है और कोई सत्यासत्य कहता है।
कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोउ मानै ।।
ये तीनों भ्रम ही हैं अर्थात् न सत्य है, न असत्य है, न सत्यासत्य है। यह कब सूझता है, जब भगवान आत्मा 'मैं' का ज्ञान हो जाता है, जब अपने आप को जान लेता है। इस पद में वे कहते हैं कि -
केशव! कहि न जाइ न कहिये ।
देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिये ।।
(पद-111)
तीन प्रकार के चित्र होते हैं -
1. चित्र, 2. विचित्र, 3. अति विचित्र ।
1. चित्र-
कागज, दीवाल, कपड़े के पर्दे आदि पर जो बने हुए रहते हैं, उन्हें चित्र कहते हैं।
2. विचित्र -
कैमरे से जो फोटो लिया जाता है, उसे विचित्र कहते हैं।
3. अति विचित्र -
तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य आदि सारा दृश्यमान जगत् यह अति विचित्र है। इसे अति विचित्र क्यों कहा? विषय समझो -
किसी भी चित्र को बनाने के लिए इतनी सामग्री आवश्यक है -
1. वह पदार्थ चाहिए जिसका चित्र बनाना है, क्योंकि उसे देखकर ही वैसा ही चित्र बनाना पड़ेगा।
2. जिस पर चित्र बनाना है वह आधार (कागज, दीवाल, कपड़े के पर्दे, बोर्ड आदि) चाहिए। यदि ये आधार नहीं होंगे तो चित्र बनाया किस पर जायेगा।
3. अन्य सामग्री जिसे चित्र बनने में लगना है-रंग, बुरुश आदि जिनके द्वारा चित्र बनाया जायेगा वह चाहिए।
4. चित्रकार चाहिए, जो चित्र को बनायेगा। जब तक ये चारों साधन उपलब्ध नहीं होंगे चित्र नहीं बन सकेगा।
चित्र और विचित्र के बनने में तो ये चारों सामग्री लगी हैं। तभी ये बने हैं, परन्तु तुम्हारे इस शरीर से लेकर पशु-पक्षी, कीट-पतंग, आदि जितने शरीर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो अतिविचित्र हैं, इनके बनने के लिए इन सामग्रियों का प्रयोग हुआ है या नहीं, इस पर विचार करना है, तब मानसकार कहते हैं कि -
सून्य भीति पर चित्र, रंग नहिं, तनु बिनु लिखा चितेरे ।
धोये मिटइ न मरइ भीति, दुख पाइअ एहि तनु हेरे ।।
तुम्हारा यह जो शरीर बना है वह किस शरीर को देखकर बनाया गया? क्या ऐसा और शरीर था, जिसे देखकर यह बनाया गया? तो निश्चय करने पर जान पड़ेगा कि ऐसा चित्र विश्व में दूसरा नहीं मिलेगा। इसी तरह प्रत्येक शरीर के बनने में उसके समान कोई भी दूसरा शरीर नहीं था, जिसे देखकर यह बनाया गया हो, पर बना है, इसलिए इसे अति विचित्र कहा कि यह बिना चित्र के ही बना है।
दूसरी चीज है, यह 'शरीर' चित्र किस आधार पर बना? तो मानसकार कहते हैं कि "शून्य भीति पर" इसका आधार भी कुछ नहीं है। तीसरी चीज-इस शरीर के बनने में रंग, बुरुश आदि कौन सी सामग्री का प्रयोग हुआ तो वह भी कुछ नहीं अर्थात् शून्य। चौथी चीज चित्रकार अर्थात् इस शरीर चित्र का बनाने वाला कौन है?
उत्तर है- 'मन' जो बिना शरीरका है और मन ने ही इसे बनाया। मृत्युकाल में प्राणी मन में जिसकी कल्पना करते-करते प्राण त्याग करता है, वह तुरन्त दूसरे जन्म में उसी शरीर का निर्माण कर लेता है, वह वही बन जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि इस शरीर का बनाने वाला चित्रकार मन है, जिसने इसे बनाया। इस तरह निश्चय हुआ जिसे देखकर यह अति विचित्र बना वह चित्र नहीं है अर्थात 'शून्य'। जिस आधार पर यह बनाया गया, वह आधार नहीं है 'शून्य भीत' पर अर्थात आधार भी शून्य।
रंग बुरुश आदि सामग्री जिसके द्वारा बनाया गया तो वह भी शून्य ही है और चित्रकार जिसने इसे बनाया तो वह चित्रकार भी "तनु बिनु लिखा चितेरे" बिना तन का है अर्थात् वह भी शून्य। तब जब चित्र शून्य आधार शून्य, सामग्री रंग, बुरुश आदि शून्य और चित्रकार (बनाने वाला) शून्य है, तब इनसे यह जो अति विचित्र, बना वह ही कैसे वास्तविक हो सकता है। अरे! वह भी शून्य ही है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त ये जो अति विचित्र है, ये सब परदेश में है। स्वदेश अर्थात् आत्मदेश में इनका अत्यन्ताभाव है अर्थात् शून्य ही है। इस तरह सारा चराचर शून्य में बना, शून्य से बना, शून्य करके बना और शून्य ही बना अर्थात् कुछ बना ही नहीं। 'मैं' आत्मा ज्यों का त्यों एक रस परिपूर्ण अपनी महिमा में नित्य स्थित हूँ। यह शून्य चैतन्य घनभूत से परिपूर्ण अनुभूति की अनुभूति है। यह किसी प्रकार धोने से नहीं मिटता, परन्तु इसको मरने का डर लगा हुआ है, वाह! कैसा आश्चर्य है।
रबिकर नीर बसै अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं ।
बदन-हीन सो ग्रसै चराचर, पान करन जे जाहीं ।
ग्रीष्मकाल में रेगिस्तान अथवा समतल विस्तृत मैदान में मृगजल दीख पड़ता है। उस मृगजल समुद्र में एक मगर रहता है। उसका मुँह नहीं है, परन्तु 'ग्रसै चराचर' वह खा जाता है-किसको? अरे! "पान करन जे जाहीं" जो उसे पान करने जाते हैं।
भगवान आत्मा के सत्तारूपी अस्तित्व में यह जो शरीर प्रपंच संसार रूपी मृगजल भासता है, जो है ही नहीं, इसको सत्य मानकर जो पान करने जाता है, उसे काल (समय) रूपी मगर, जो बिना मुँह का है, खा जाता है। अभी 'शरीर' अति विचित्र शून्य है, है ही नहीं, यह अनुभव किया गया अब इस शरीर को सत्य मानना कि यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा मानना ही मृगजल को पान करने जाना है। तो उन्हीं को काल रूपी मगर खाता है। मोह रूपी वन में विचरने वाले मनुष्य मृगरूप, जो संसारी अज्ञानी जीव हैं, वे ही इसे सत्य मानकर पान करते हैं, जिन्हें काल रूपी मगर निगल जाता है।
कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोउ मानै ।
तुलसिदास परिहरै तीन भ्रम, सो आपन पहिचानै ।।
संसार न तो स्वयं पैदा हुआ है और न किसी ने इसे पैदा किया है। यदि कहो कि संसार स्वयं पैदा हुआ है तो पैदा होने के पहिले यह सत्य था या असत्य था? यदि, कहो सत्य था तो सत्य की तो उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति मानने पर उसका विनाश मानना पड़ेगा, फिर वह सत्य न रहा। यदि असत्य कहो तो असत्य तो बन्ध्या का पुत्र होता है। अभाव रूप जो है ही नहीं, वह क्या पैदा होगा? यदि सत्यासत्य कहो तो साधक-बाधक पदार्थ साथ-साथ नहीं रह सकते। प्रकाश और अन्धकार एक साथ नहीं रहते। अब कहो कि इसे भगवान ने पैदा किया तो जिस भगवान ने इसे पैदा किया वह परमात्मा जन्मा है या अजन्मा है? यदि अजन्मा मानोगे तो वह एक दिन मरेगा, क्योंकि जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता है, फिर वह अविनाशी न हुआ। अब अजन्मा भगवान ने पैदा किया कहो तो जो स्वयं पैदा नहीं हुआ उसे क्या तमीज है जो दूसरों को पैदा करेगा। इस तरह संसार न सत्य है, न असत्य है, न सत्यासत्य है। ये तीनों भ्रम ही हैं। किसी भी प्रकार से संसार की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, संसार हुआ ही नहीं। अब प्रश्न होता है कि फिर शास्त्रों में संसार का होना बताया गया है, वह क्या है? उत्तर है- अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए शास्त्रों ने पहिले निष्प्रपंच ब्रह्म, भगवान आत्मा में संसार प्रपंच का अध्यारोप किया। अभाव में भाव की उत्पत्ति बतायी और उसी शास्त्र में आगे चलकर किये गये अध्यारोप का अपवाद (खण्डन) कर दिया गया।
ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। द्रष्टा, दृश्य, दर्शन जहाँ तक तीन है अर्थात् त्रिपुटी इन्हें 'परिहरहु' इनका त्याग कर दो, जब इनका त्याग कर दोगे तब 'आपन पहिचाने' तब अपना स्वरूप 'मैं' आत्मा भगवान का ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं।
'जोग-बियोग भोग भल मन्दा, हित अनहित मध्यम भ्रम फन्दा' से लेकर 'मोह मूल परमारथु नाहीं' तक ये सब मन की ही बीमारी है। मन स्वयं रोग है। मन रोग के कारण ही जीव, ईश्वर, ब्रह्म, जगत्, मैं, तू, अपना, पराया, जड़-चेतन आदि का भेद रूपी सब रोग पैदा होते हैं। गाढी नींद में यह मन जब नहीं रहता तब ये सब भेद भी नहीं रहते। शुद्ध तत्त्व 'मैं' का 'मैं' आत्मा ही रहता हूँ। मन कितना चंचल रहता है, यह सब जानते हैं। मन को रोकने के लिए ही 'योगदर्शन' एक दर्शन ही बना है। बड़े से बड़े साधन इस मन को रोकने के लिए किये जाते हैं, फिर भी यह मन काबू में नहीं होता। श्री मानसकार विनय में कहते हैं -
मेरो मन हरिजू! हठ न तजै ।
निसिदिन नाथ देउँ सिख बहु बिधि, करत सुभाउ निजै ॥
ज्यों जुबती अनुभवति प्रसव अति, दारुन दुख उपजै ।
है अनुकूल बिसारि सूल सठ, पुनि खल पतिहिं भजै ॥
लोलुप भ्रम गृह पसु ज्यों जहँ तहँ, सिर पदत्रान बजै ।
तदपि अधम विचरत तेहि मारग, कबहुँ न मूढ़ लजै ॥
(पद 89)
वे कहते हैं कि हे हरि! मेरा मन अपनी आदत नहीं त्यागता। मैं रात-दिन इसे अनेक प्रकार से समझाता हूँ, पर यह अपनी ही आदत के अनुसार चलता है। जैसे, युवती स्त्री संतान जनने के समय अत्यन्त असह्य कष्ट का अनुभव करती है, उस समय वह मन में निश्चय करती है कि अब भविष्य में मैं पति के पास नहीं जाऊँगी और पुनः ऐसा प्रसंग न आने दूंगी, परन्तु वह मूर्खा समय टल जाने पर सारी वेदना को भूलकर उसी दुःख देने वाले पति का सेवन करती है। ऐसे ही, रोटी के टुकड़े का लालची कुत्ता जहाँ जाता है, उसके सिर पर जूते पड़ते हैं तो भी वह नीच उसी रास्ते भटकता है और जरा भी लज्जित नहीं होता। ऐसी ही दशा मेरे मन की है। विषयों में कष्ट पाने पर भी यह उन्हीं की ओर दौड़-दौड़कर जाता है।
हौं हारयो करि जतन बिबिध बिधि, अतिसै प्रबल अजै ।
तुलसिदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजै ॥
मानसकार कहते हैं कि मैं इसके लिए अनेक उपाय कर चुका और साधन करके थक गया, परन्तु यह मन बड़ा बलवान और अजेय है, यह वश में नहीं होता। यह वश में तो तभी हो सकता है, जब इसे इसको प्रेरणा देने वाला इसका शासक जो प्रेरक है, वह ही इसे रोके। अच्छा, तो चलो अब विचार वाटिका में थोडा घूमें।
मन को साधन के द्वारा वश में नहीं कर सकते, जब इसे इसका प्रेरक प्रभु समझायेगा तब यह अपने आप वश में हो जायेगा।
प्रश्न होता है कि इसका प्रेरक प्रभु कौन है। उत्तर है- जो कहता है कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है, वही उसका प्रेरक (स्वामी) है। देखो-अभी जब तुम कथा सुन रहे हो तब तुम्हारा मन तुम्हारे में काबू में है या नहीं? यदि मन काबू में नहीं रहेगा तो तुम कथा सुन नहीं सकते, पर सुन रहे हो इससे सिद्ध है कि तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है। इसे वश में करने के लिए तुम घर से कौन-सा साधन करके चले थे अथवा यहाँ आकर तुमने कौन सा साधन किया है, जिससे कि तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हुआ? इसका उत्तर है कि कुछ भी साधन नहीं किया गया यह अपने आप वश में है।
विषय समझो - मन जब वश में होता है, तभी संसार के सब काम होते हैं। जब तुम सिनेमा देखने जाते हो तब घर से कौन-सा साधन करके जाते हो कि तीन घंटे तक कुर्सी पर ऐसे मूर्तिवत् बैठे रहते हो मानों किसी ने काठ की पुतली बनाकर बिठा दिया हो। इसके लिए क्या ध्यान, धारणा अथवा समाधि लगाकर जाते हो। दुकान में घंटों बैठे हुए एक-एक पाई का रोकड़ मिलाते हो। दफ्तर में बड़े से बड़े काम करते हो, अदालत में वकालत करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म तर्क करते हो आदि। यदि इन कामों के करते समय तुम्हारा मन तुम्हारे वश में न रहकर उद्विग्न, चंचल, अस्थिर रहे तो क्या तुम ये सब काम कर सकते हो? कदापि नहीं, पर सब काम ठीक-ठाक होते रहते हैं। कहीं पर कुछ भी भूल नहीं हो पाती। अब विचार करना है कि इस तरह मन, जो अपने वश में रहता है, वह साधन से वश में रहता है या बिना साधन के ? उत्तर मिलेगा, बिना साधन के मन वश में रहता है, क्योंकि इसे वश में होने के लिए मैंने कोई साधन नहीं किया। फिर भी, वश में रहा। तब मन बेकाबू (वश से बाहर) कब हो जाता है? जब मैं अपने आप को कुछ मान लेता हूँ। इसका प्रमाण लो -
अभी कथा सुनने बैठे हो और कथा सुन रहे हो, तब अपने आप को कुछ मानकर कथा सुन रहे हो या बिना कुछ माने स्वाभाविक ? उत्तर है- बिना कुछ माने स्वाभाविका विषय को खूब समझ लो, यह कंगाल पद नहीं सम्राट पद है। जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन विषयों का अनुभव करते हो, तब मन वश में रहता है या बेवश रहता है। तब अनुभव करते हो? उत्तर है- मन वश में रहता है, तभी अनुभव होता है। प्रश्न होता है, यह साधन से वश में हुआ रहता है या बिना साधन के ?
उत्तर मिलेगा- बिना साधन किये वश में रहता है, इसका रहस्य समझो जब 'मैं' का 'मैं' ही रहता हूँ, अपने 'मैं' को कुछ नहीं मानता तब यह मन अपने आप वश में रहता है और जब में अपने 'मैं' को कुछ मान लेता हूँ, मैं देह हूँ, जीव हूँ, ब्रह्म हूँ आदि तब मन काबू से बाहर हो जाता है। 'मैं' को कुछ माना कि मन तुम्हार र बाली हो गया और 'मैं' के माने 'मैं' ही हूँ। इस भाव में मन का स्वामी 'मैं' हूँ।
अज्ञानियों के लिए मन को रोकने के लिए कुछ करना जितना सरल है। बोधवान के लिए उसे रोकने के लिए कुछ करना उतना ही कठिन है। इसीलिए, अज्ञानी मन को रोकने के लिए कुछ न कुछ साधना करते रहता है। यह मन साधन से वश में नहीं होता। संसार में संत तुलसीदास जैसे साधक कौन होगा? जो कहते हैं कि -
हौं हार्यो करि जतन बिबिध बिधि, अतिसै प्रबल अजै ॥
सब कुछ साधन करके मैं थक गया, परन्तु यह मन वश में नहीं हुआ। तो भैय्या! यह मन वश में तभी होता है जब इसका प्रेरक भगवान आत्मा 'मैं' की इस पर कृपा होती है अर्थात् अपने 'मैं' भगवान आत्मा का बोध हो जाता है, बिना बोध हुए यह मन वश में नहीं होता।
'मैं' हूँ इस भाव में तो मन नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब मैं अपने आपको कुछ मानता हूँ, तभी मन पैदा हो जाता है। मैं ही इसे पैदा कर लेता हूँ और फिर इसे रोकने का साधन करता हूँ। जितने साधन हैं, इससे मनरूपी बीमारी दब जाती है। जड़ सहित नाश नहीं होती, इसे जड़ सहित नाश करने की एक ही दवा है और वह दवा यह है कि मन नाम की कोई चीज ही नहीं है।
मन है ही नहीं। बशर्ते कि अपने आपको देह मान्यता, जीव मान्यता आदि से रहित होकर देखो। बीमारी का कारण मान्यता ही है। बल्कि, मान्यता ही मन है। सांसारिक विषयों के अनुभव काल में मैं अपने को कुछ नहीं मानता। में जैसा हूँ, जो हूँ, जहाँ हूँ, वैसा ही, वही और वहाँ ही रहता हूँ। इसलिए, कुछ भी विक्षेप नहीं होता, मन नहीं रहता, परन्तु जब मैं अपने आपको पुजारी, ध्यानी आदि मान लेता हूँ, तब इस मान्यता में मन पैदा हो जाता है और पूजा, पाठ, ध्यान, धारणा में मन चंचल हो उठता है, फिर तो उस समय पुराने-पुराने मरे हुए पुरखे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिनकी इस समय यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मन है नहीं तब तो इतनी परेशानी है और यदि होता तो क्या होता?
अरे! यदि यह होता तो 'मैं' ही होता, डण्डा है नहीं और यदि डण्डा है तो लकड़ी ही है। जहाँ तक मन जाता है, वहाँ तक संसार है, परन्तु 'मैं' आत्मा कहाँ तक हूँ, इसकी कोई सीमा नहीं है।
मन के निरोध करने के लिए, रोकने के लिए तो साधन है, पर इसे स्थिर करने के लिए कोई साधन नहीं है। नदी को रोकने के लिए तो साधन है। बाँध आदि बनाकर यह रोकी जा सकती है, परन्तु इसे स्थिर करने का कोई साधन नहीं है। स्थिर तो यह समुद्र में पहुँचकर ही होगी। इसी तरह मन स्थिर तो तभी होगा जब यह आनन्द सागर सुख सिन्धु में पहुँच जायेगा।
यदि तुम अपने को संसारी जीव मानते हो, तब तो मन को रोकने का साधन करो और यदि अपने आपको आत्मा जानते हो तो कुछ भी साधन मत करो। किसी प्रकार का साधन करना मन के अस्तित्व को मानना है और कहा जा चुका है कि मानना ही मन है। कुछ भी मान लेना ही मन की उत्पत्ति कर लेना है। जीव कहो या मन कहो दोनों एक ही हैं। मन का ही दूसरा नाम संसार है।
मन माया प्रकृति जगत, चार नाम इक रूप ।
तब लगि ये साँचो लगै, नहि जाना निज रूप ।।
मन के अभाव में संसार का अभाव है और मन के उदय में संसार प्रपंच का उदय है। चंचलता का नाम ही मन है। चंचलता रहित अवस्था 'मैं' आत्मा ही है। चंचलता ही लहर है, इससे रहित जल ही है। इसी तरह जब तक संकल्प-विकल्प रूपी लहर है, तभी तक मन है। इससे रहित अवस्था ही आत्मा है। मन लहर के समान अपने आप में विलीन हो जाता है, तब वह आत्मा ही है। लहर, पहिले भी तो जल ही था। सिवा जल के लहर अलग है कहाँ? अपने आपका ही नाम मन है।
मन है नदी। कल्पना है धार और एकाग्रता बाँध है। मन शुद्ध है तो 'मैं' ही हूँ और मन अशुद्ध है तो मन है। मन रूपी पारा को 'मन क्या है, कैसा है, कौन है' इस विचार रूपी नली से पकड़ो फिर 'मन है ही नहीं' इसे वैराग्य रूपी जड़ी से मूच्छिंत करो, फिर इसे अभ्यास रूपी औषधि से मार दो।
सर्व ब्रह्म है 'अहमेवेदं' उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं, इस अग्नि से भस्म कर लो, फिर तो सर्व भवरोग नाशक औषधि तैयार हो जायेगी, जो सम्पूर्ण भवरोग की रामबाण दवा होगी। मन को रोकना कठिन है। उसे स्थिर करना कठिन नहीं है। प्रश्न होता है, रोकना क्यों कठिन है? इसलिए, कठिन है कि साधक इसे रोकने के लिए ज्यों-ज्यों साधन करता है, त्यों-त्यों यह और भी चंचल होता है। इसकी जड़ मजबूत होते चलती है, क्योंकि साधन करने वाला 'मन है' ऐसा मानकर ही तो साधन करता है, इससे इसकी जड़ ही तो मजबूत हुई।
अभ्यास और वैराग्य से ही मन पकड़ा जाता है। मन, वचन, कर्म के द्वारा एक ही काम को बार-बार करने का नाम अभ्यास और मन, वचन, कर्म के द्वारा दुःख रूप प्रपंच के त्याग का नाम वैराग्य है। अनभ्यास के अभ्यास का नाम अभ्यास है और विषय प्रपंच के अस्तित्व के त्याग का नाम वैराग्य है। मन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करना यही अभ्यास है, इसी को अनभ्यास कहते हैं। अगर, मन को जिन्दा रखना है तो उसके लिए अभ्यास करो और उसे मार डालना है तो उसके लिए कुछ भी मत करो। तुम्हारे नित्य के सर्व व्यवहारिक कार्य, अभी कथा का सुनना, सिनेमा देखना, रोकड़ मिलाना, कचहरी कोर्ट, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, व्यापार, व्यवसाय आदि सभी कार्य अनभ्यास में ही हो रहे हैं। इस समय मन नाम की कोई चीज ही नहीं है। यही मन को रोकने के लिए कुछ नहीं करना, अनभ्यास है। अनभ्यास से ही मन काबू में होता है, इसका यही प्रत्यक्ष प्रबल प्रमाण है। अभ्यास से जो आनन्द की अनुभूति होती है, वह क्षणिक आनन्द है, अनित्य सुख है। अभ्यास से विषयानन्द की प्राप्ति होती है और अनभ्यास से आत्मानन्द की प्राप्ति होती है। जीव देश में अभ्यास का अभ्यास होता है। अनभ्यास का अभ्यास करने के लिए जीव देश को छोड़कर आत्मदेश में आना पड़ेगा, तभी यह अनभ्यास का अभ्यास हो सकेगा। जीव देश का निवासी ऐसा करने में समर्थ नहीं है। जीव देश का निवासी मान्यता का पुजारी होता है और आत्मदेश का निवासी जानने का पुजारी होता है।
अनुभव काल में 'मैं' आत्मा होकर, आत्मदेश में रहकर अनुभव करता हूँ और, जब 'मैं' जीव बनता हूँ, तब सामने मन दिखाई देता है। उसे मारने के लिए, जीतने के लिए कुछ करना पड़ता है। आत्मदेश में मन नाम की कोई चीज ही नहीं रहती, रोकेंगे किसको? अनुभव करना भगवान आत्मा का काम है। अतः, अनुभवकाल में 'मैं' जैसा हूँ, वैसा ही रहता हूँ। जीव बनकर साधन करता हूँ, आत्मा होकर अनुभव करता हूँ।
अनभ्यास की स्थिति में प्रपंचाभाव का अनुभव होता है और अभ्यास की स्थिति में प्रपंच का दर्शन होता है। अनभ्यास में सभी व्यवहार होते हुए नहीं होते हैं और अभ्यास में व्यवहार नहीं होते हुए होते हैं।
स्वरूप स्थिति अनभ्यास काल का फल है। अभिमान रहित होकर बालकवत् सब कार्य व व्यवहार करते रहना, यही अनभ्यास का स्वरूप है। बालक खेलता है, खाता-पीता है, बोलता है, हँसता है, रोता है, परन्तु उस पर उसका अभिमान नहीं रहता। इसका फल यही है कि यदि कुबेर का खजाना भी मिल जाय अथवा पथ का भिखारी हो जाये तो हृदय में ग्लानि की रेखा भी न पड़े।
मन से युद्ध करके विजय प्राप्त करने की अपेक्षा उससे समझौता करके समस्या को सुलझाना अधिक हितकर होता है। मन के विरोध के जितने साधन हैं, वह तो उससे युद्ध करना है, इसलिए साधन का मार्ग न अपना कर इस तरह समझौता करे।
उत्तम पुरुष 'मैं' के बिना किसी भी देश, काल, वस्तु की सिद्धि नहीं, इसलिए मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। सारा चराचर बिना 'मैं' के अपनी सिद्धि यदि कर लेता है तब तो सारा चराचर है और यदि बिना 'मैं' के अपनी सिद्धि नहीं कर सकता तब 'मैं' ही हूँ, जिसे सारा चराचर कहते हैं। यदि डण्डे से तुम पूछोगे कि तुम कौन हो? तो वह भी यही कहेगा कि मैं डण्डा हूँ, तब 'मैं' ही हूँ जिसका नाम डण्डा है, क्योंकि 'मैं' के बिना डण्डा भी अपनी सिद्धि नहीं कर सकता। इसी तरह, यदि मन से पूछोगे कि तुम कौन हो? तो वह भी यह उत्तर देगा कि 'मैं' मन हूँ, तब 'मैं' ही हूँ, जिसका नाम मन है। जब 'मैं' ही मन हो गया, तब मन का माना हुआ सारा चराचर मैं ही हुआ। ऐसा विचार करना ही मन से समझौता करना है। इस विवेकिनी बुद्धि से मन मुझ आत्मा में विलीन हो गया। यही मन पर विजय पाना है। किसी भी विषय के विषयकाल में क्या यह भान रहता है कि मैं अमुक हूँ, यह विषय है और मैं विषय कर रहा हूँ (ठीक अनुभव करते समय, थोड़ा भी आगे-पीछे नहीं) इन तीनों का अभाव रहता है, केवल अनुभव ही अनुभव रहता है। इस अवस्था में न कर्त्ता है, न कर्म है और न क्रिया है केवल अनुभव ही अनुभव है। केवलानुभवानन्द यह अवस्था आत्मस्वरूप ही है। यही 'मैं' आत्मा हूँ।
मन रूपी गौ के लिए पंचादिक विषयरूपी घास है, जब मन ही न रहा, तब विषय रूपी चारा ही कहाँ रहा।
"जोग-बियोग भोग भल मन्दा" से लेकर "सरगु नरकु जैह लगि ब्यवहारू" तक ये सब मन के अन्दर है। इन्हें मन ने ही माना है, जब मन का ही अत्यन्ताभाव है, तब उपरोक्त सब प्रपंच ही कहाँ? न तो इन्द्रियाँ एक समय में अनेक काम करती हैं और न मन एक ही समय में अनेक काम करता है, अतः सिद्ध है कि मन ही एक प्रमुख इन्द्रिय है। जब वह श्रवण क्रिया करने लगता है, तब उसी मन का नाम कर्ण इन्द्रिय हो जाता है और जब देखने की क्रिया करता है तब आँख अर्थात चक्षु इन्द्रिय हो जाता है। अतः, इन्द्रियाँ अनेक नहीं हैं केवल एक ही है, जिसका नाम मन है।
मन को माना 'मैं' ने और मन ने माना जगत् को। मन का स्थूल रूप शरीर है। और मुझ आत्मा का स्थूल रूप मन है।
मन को जान लिया तो शरीर नहीं और 'मैं' को जान लिया तो मन नहीं। जिस प्रकार जल के ज्ञान में लहर का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार 'मैं' के ज्ञान में नवका अस्तित्व नहीं। अपने आप को जानो तब मन नहीं और मन को जानो तब मन नहीं। जल को जानो तब लहर नहीं और लहर को जानो तब लहर नहीं। लहर को पर नहीं। तो क्या लहर मिलेगी? नहीं जल ही हाथ आयेगा।
मन 'मैं' आत्मा का सांकल्पिक पुत्र है, जीव इसे साधन के बल पर जीतना चाहता है, क्या जीव की ताकत है वह उसे जीत सके? असम्भव।
जीवदेश में यह मन, मन है और 'मैं' देश में यह मन 'मैं' आत्मा है।
मन की स्थापना किया 'मैं' आत्मा ने, तब भगवान आत्मा का पुत्र जो मन है वह 'मैं' के अनुशासन में रह सकता है, जीव के अनुशासन के भीतर वह आ ही नहीं सकता। मन का अस्तित्व मानने पर मन पर विजय नहीं, मन का अस्तित्व जानने पर मन पर विजय है।
मन के अभाव में ही प्रपंच का अभाव है। मन रूपी नदी जीव देश में रुकती है और आत्मदेशमें शांत होती है। यह मन कुछ करने से तो रुकता है और कुछ न करने से स्थिर हो जाता है।
रुकने में मन का अस्तित्व है और स्थिरता में उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सर्व के मन के बहाव का एक ही लक्ष्य है, वह है नित्यानन्द की प्राप्ति। कूकर, शूकर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणिमात्र का सबके मन का प्रवाह एक ही ओर है, अतः सिद्ध है कि मन एक ही है।
आत्मा भी एक ही है और मन भी एक ही है, सबका शरीर एक पंचमहाभूतों से बना है। अतः, शरीर भी एक ही है, अनेक नहीं। इस तरह एक ही है, जो सर्व है। इस अनुभूति में सर्व न रहा, एक ही रहा। जब सर्व न रहा, तब एक भी न रहा, सर्व के लिए ही तो एक कहा गया, तब क्या रहा? बस, जो रहा वह न सर्व है, न एक है। जो है, सो है। जैसा है, वैसा है।
'मैं' हूँ इसकी अनुभूति प्राणिमात्र को है, सदैव 'मैं' हूँ इसका ही अनुभव प्रत्येक करता है, अमुक हूँ का नहीं।
'मैं' हूँ इस भाव में मन काबू में है, 'मैं' अमुक हूँ इस भाव में मन कभी भी काबू में नहीं रह सकता।
जैसे ब्रह्म अक्रिय है, इसी तरह मन भी अक्रिय ही है, इन दोनों का प्रयोग व्याकरण शास्त्र में नपुन्सक लिंग में हुआ है। मन न कहीं जाता है, न आता है, अनन्त जन्मों के दृश्यों और कृत्यों के चित्र अन्तःकरण चित्रशाला में टंगे हुए हैं, इन्ही को वह समय-समय पर पलट-पलटकर देखा करता है, इसी को लोग मन का आना-जाना मानते हैं।
चिन्हारी दृश्यानुभूति है, विकल्प का अभाव भासानुभूति है, सर्व भावों का अभाव स्वात्मानुभूति है। न किसी का भाव करो, न किसी का अभाव, यही स्वात्मानुभूति है, यहाँ न सूक्ष्म है, न स्थूल, न जड़ है, न चेतन।
श्रुति कहती है कि यदि बन्ध्या का पुत्र शेर का शिकार कर सकता हो, खरगोश के सींग हो सकते हों, गीले केले के खम्भे में भोजन पकाया जा सकता हो, अभी की पैदा हुई कन्या गर्भवती हो सकती हो, नपुंसक कुमार से यदि स्त्री को भोग सुख मिल सकता हो, यदि उपरोक्त सब हो सकते हों, तब तो समझो कि मन है, अन्यथा मन है ही नहीं। इसलिए, भैय्या निषाद।
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारथु नहीं ।
यहाँ तक ज्ञान का प्रसंग है।
सपने होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ ।
जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जियँ जोइ ।।
यहाँ से वैराग्य का प्रसंग शुरू होता है। जैसे स्वप्न में राजा अपने को भिखारी हुआ देखे और भिखारी अपने को इन्द्र हुआ देखे, परन्तु जागने पर न कुछ लाभ हुआ, न कुछ हानि हुई। राजा, राजा ही है और भिखारी, भिखारी है। इसी तरह यह जगत् प्रपंच का स्वप्न है।
मोह निसाँ सबु सोवनिहारा । देखिअ सपन अनेक प्रकारा ।।
जितने सब संसारी जीव हैं, वे मोह निशा अर्थात् अज्ञान की रात्रि में सो रहे है और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं।
अस्तित्व, भगवान आत्मा को शरीर मानना यही स्वप्न है और शरीर मानकर शरीर के धर्मों को अपने आप में मानना यह सपने के अंदर सपना है। अर्थात् स्वप्नान्तर है। पहिले 'मैं' शरीर हूँ माना यह हुआ स्वप्न, फिर इस मान्यता के बाद इसके धर्मों को अपने में माना, में स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हैं, पिता, पुत्र, भाई, बहिन, माता, काका, मामा आदि हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र हूँ। गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी सन्यासी हूँ आदि माना, यह हुआ स्वप्नान्तरा 'मैं' संसारी जीव हूँ इस मान्यता में 'मैं' अस्तित्व को जीव माना यह हुआ स्वप्न। इसके बाद मैं आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सुखी हूँ, दुःखी हूँ, स्वर्गी हूँ, नरकी हूँ आदि जीव के धर्मों को अपने में मानना स्वप्नान्तर है। ये स्वप्न और स्वप्नान्तर दोनों मोह की नींद का स्वप्न है।
प्रश्न है- स्वामी जी! इसको तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ और आप इसे स्वप्न कहते हैं, तो इसे मैं कैसे मानूं?
उत्तर है- भैय्या! देखो जब तुम स्वप्न देखते हो तब उस समय तुम्हें क्या यह अनुभव होता है कि जो मैं देख रहा हूँ वह स्वप्न है, असत्य है, उसे भी तो प्रत्यक्ष देखते हो। मगर ऐसा अनुभव नहीं होता। उस समय यदि कोई तुम्हें समझावे कि भाई! यह जो तुम देख रहे हो वह स्वप्न है, जागने पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तब तुम नहीं मानोगे, क्योंकि उस समय प्रत्यक्ष सत्य अनुभव कर रहे हो। स्वप्न है यह तो जागने पर ही जाना जाता है। जागने पर बिना किसी के समझाये तुम स्वयं कहने लगते हो कि अरे! वह स्वप्न था, जिसे मैं देख रहा था। इसी तरह अभी जो तुम प्रत्यक्ष देख रहो हो वह अज्ञान की रात्रि में स्वप्न देख रहे हो। यह तुम्हें असत्य तो तभी अनुभव होगा, जब तुम स्व स्वरूप भगवान आत्मा में जाग जाओगे। तबला चिकारा में रात-दिन रामायण गा रहे हो कि -
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना, सत हरिभजनु जगत सब सपना ।
सीय राम मय सब जग जानी, करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ।।
तो इसका अनुभव क्यों नहीं हो जाता? वह इसलिए कि तुम्हारा गाना बजाना और पढना भी सपने में ही हो रहा है।
महाराज जनक ने एक बार अपने राजमहल में सोये हुए स्वप्न देखा कि मेरे राज्य में पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है। उसके साथ में युद्ध में हार गया हूँ और मेरे राजपाट, कोष, सेना, दास-दासियाँ आदि सब पर उसका अधिकार हो गया है। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया है। मैं पथ का भिखारी हो गया हूँ। मेरे पास शरीर में सिर्फ एक धोती, जिसे कि में पहिने हुए हूँ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। मैं इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा हूँ। इसी स्थिति में मुझे तीन दिनों तक खाने को कुछ नहीं मिला है। मैं भूख से अत्यन्त व्याकुल हो रहा हूँ। इतने में क्या देखता हूँ कि सामने क्षेत्र में भिखारियों की भीड़ लगी हुई है और वहाँ खिचडी बँट रही है। मैं भी कहीं से पड़ी हुई मिट्टी की हण्डी उठा लाया और उसमें क्षेत्र से खिचड़ी मांगकर ला रहा था कि एकान्त में किसी पेड़ की छाया में बैठकर खिचड़ी खाकर अपनी भूख मिटाऊँ कि इसी बीच दो साँड लड़ते हुए मेरे समीप आये और वे मुझसे टकरा गये, जिससे मेरे हाथ में रखी हुई वह खिचड़ी की हण्डी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी जिससे हण्डी फूट गयी और सब खिचड़ी बिखर गयी। मैं अत्यन्त भूख से व्याकुल दुःख के साथ झाड़ के नीचे आकर बैठ गया हूँ। वह ऐसा स्वप्न देख ही रहा था कि घबराहट में उसकी नींद खुल गयी और वे जाग उठे।
जाग जाने पर उन्हें स्वप्न का सारा दृश्य आँखों के सामने प्रत्यक्ष दिखने लगा। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और वे सोचने लगे कि मैं अभी-अभी पथ का भिखारी था, न भोजन की व्यवस्था थी, न वस्त्र का ठिकाना था। भूख से व्याकुल इधर-उधर मारा- मारा भटक रहा था और अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं राजभवन में हूँ। राजपाट, रानियाँ, दास-दासियाँ, मंत्री, प्रजा, सेना, कोष सब हैं, तब अभी-अभी जो मैं भिखारी जनक था वह सच है अथवा इस समय जो में अपने को राजा जनक अनुभव कर रहा हूँ, यह सच है। इन दोनों में कौन सच है? बस, इसी चिन्ता में पड़े-पड़े उसने बड़ी कठिनाई से शेष रात बिताई।
प्रातःकाल होते ही उसने दरबार लगाने की आज्ञा दी। दरबार में जब सब दरबारी और मंत्रिमंडल आकर बैठ गये, तब उसने मन में सोचा कि यदि मैं अपने स्वप्न का सारा हाल उन्हें बताता हूँ तो यह मेरे लिए बडी लज्जा की बात होगी और इसमें मुझे अपमानित होना पड़ेगा। अतः, उसने दरबारियों और मंत्रियों से कहा कि मेरे सामने एक प्रश्न है, इसका संतोषजनक उत्तर जो कोई मुझे दे देगा, उसे में अपना आधा राज्य दे दूंगा। मेरी इस घोषणा की राज्य भर में डांडी पिटवा दी जाय। तत्पश्चात् उसने दरबारियों के समक्ष अपना यह प्रश्न रखा, प्रश्न केवल इतना ही था कि -
यह सच है कि, वह सच है।
दरबारियों की समझ में कुछ बात नहीं आयी और वे उसका कुछ उत्तर न दे सके। इस घोषणा के अनुसार रोज बहुत से विद्वान ऋषि-मुनि उनके दरबार में आते और इस प्रश्न का उत्तर देते, पर राजा को किसी से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। उन्होंने सब विद्वानों और ऋषियों को अपने यहाँ बन्दी बना लिया और उनकी आदरपूर्वक सेवा करते हुए उन्हें इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं आराम से रहते हुए इस प्रश्न का उत्तर सोचिये और मेरा समाधान कीजिये। यहाँ आप लोगों की हर तरह से आराम और सुख-सुविधा की व्यवस्था रहेगी। इसी प्रसंग में उनके यहाँ अष्टावक्र जी का शुभागमन हुआ, जिसका शरीर आठ जगह से टेढ़ा था और जो कहोल ऋषि के पुत्र थे। कहोल भी राजा जनक के यहाँ बन्दी थे। जब बालक अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में ही थे तब एक दिन कहोल ऋषि वेद पाठ कर रहे थे और उनकी गर्भवती धर्मपत्नी उनके पास बैठी चावल चुन रही थी।
कहोल ऋषि के सस्वर पाठ करने में कुछ अशुद्ध पाठ हुए, जिसे बालक ने माता के गर्भ से ही टोक दिया। इस तरह जब उसे आठ बार टोकते हो गया तब पिता को क्रोध आ गया वे जान गये कि यह गर्भ स्थित बालक ही मुझे टोक रहा है। उसने उसे तत्काल श्राप दिया कि जब अभी से तुझे अपनी विद्वत्ता का इतना अभिमान है कि मेरी अशुद्धि निकाल रहा है तो जा तू आठ जगह से टेढ़ा हो जा। बस, इसी श्रापवश उनका शरीर गर्भ में ही आठ जगह से टेढ़ा हो गया। वे माता के गर्भ से इसी तरह पैदा हुए, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इतिहास बड़ा लम्बा है कहाँ तक कहें। निदान राजा जनक ने उनकी विधिवत् पूजा की उनके समक्ष नम्रतापूर्वक अपना वही प्रश्न रखा। प्रश्न सुनकर सप्तवर्षीय अष्टावक्र ने उनसे कहा कि ऐ जनक! तुम्हारा प्रश्न है कि "यह सच है, कि वह सच है" तो जैसा तेरा संक्षिप्त प्रश्न है, वैसा ही संक्षिप्त उत्तर इसका यही है कि "न यह सच है, न वह सच है" और इसका विस्तृत उत्तर सुनना है तो वह भी सुन। ऐसा कह उन्होंने दरबारियों के समक्ष राजा के उस देखे हुए स्वप्न का पूरा-पूरा विवरण कह सुनाया। इसके बाद वे कहने लगे कि सत्य वह है, जो तीनों काल (भूत, भविष्य और वर्तमान) और तीनों अवस्था (जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति) में नित्य एक रस रहे, उसका किसी क्षण भी अभाव न हो। तुमने जो भिखारी जनक देखा था, वह जनक अभी वर्तमान में नहीं है, भविष्यकाल में भी उसका अभाव है, जागृत और सुषुप्ति अवस्था में भी वह नहीं है। अतः, वह सच नहीं है। इसी तरह अभी जो जनक हो वह स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं। भूतकाल और भविष्यकाल अर्थात् सौ हजार वर्ष बाद नहीं रहने वाला है। अतः, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि तीनों काल और तीनों अवस्था में कभी न कभी इनका अभाव है। अतः, दोनों असत्य है। इसलिए, न यह सच है, न वह सच है। जागृत अवस्था के सब प्रपंच स्वप्न अवस्था में नहीं रहते और स्वप्न अवस्था के सब प्रपंच जागृत अवस्था में नहीं रहते। अतः, न यह सच है, न वह सच है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था नहीं और स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था नहीं। अतः, दोनों असत्य। दोनों जगत् स्वप्न है।
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरिभजनु जगत सब सपना ।।
प्रश्न है - तब सत्य क्या है?
उत्तर है- अरे! जो इसे भी देखता है और उसे भी देखता है, वही सत्य है। जागृत अवस्था के सब प्रपंच को और स्वप्न अवस्था के सारे प्रपंचों को जो सुषुप्ति अवस्था में अपने में समेटकर चैतन्यरूप से नित्य विद्यमान रहता है वह 'मैं' आत्मा ही सत्य है। तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी, दृष्टा और अनुभव करने वाला 'मैं' आत्मा ही है, वही सत्य है। जनक के द्वारा किये गये अनेक प्रश्नों का महात्मा अष्टावक्र ने विलक्षण उत्तर दिया। जिससे, राजा जनक बड़े प्रभावित हुए और उनके ही उपदेश से राजा जनक को आत्मतत्त्व का बोध हुआ। तदनन्तर, उनकी ही आज्ञा से बन्दी हुए ऋषियों और मुनियों को छुटकारा मिला।
अपने आत्मा 'मैं' को संघात मानना स्वप्न है और आत्मा 'मैं' में संघात के धर्मो को मानना स्वप्नान्तर है। 'मैं' के सिवा जो भी है सब संघात है।
मान्यता जगत् का नागरिक मोह निशा में सोता है और आत्मदेश का नागरिक मोह निशा में जागता है।
मोह निसाँ सबु सोवनि हारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा ।
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच बियोगी ।।
इस रात्रि में योगी जागते हैं, कौन योगी? जो परमारथी हैं और जिनने प्रपंच का त्याग कर दिया है वे। परमार्थी का अर्थ होता है, परम + अर्थी अर्थात् परमार्थी। तो परमार्थ तो सिर्फ 'मैं' आत्मा ही है। इसमें जो नित्यरत है, वह है परमार्थी। जिसकी दृष्टि में भगवान आत्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। 'वासुदेवं सर्व', 'नारायणेवेदं सर्व', 'आत्मैवेदं सर्व', 'ब्रह्मवेदं सर्व' में जो रत है। इस प्रकार की जब अनुभूति होने लगे तब जानो कि जीव जग गया है। इस स्वरूप के बोध में फिर संसार का अभाव हो जाता है अर्थात् जगत् प्रपंच का स्वप्न मिट जाता है। तब समझ में आता है कि जगत् स्वप्न है। उसे फिर समझाना नहीं पड़ता कि यह स्वप्न है।
जानिअ तबहिं जीव जग जागा, जब सब विषय बिलास बिरागा ।।
जीव संसार में जग गया तभी जानो जब उसे विषय और उसके विलास से वैराग्य हो जाय।
वैराग्य दो प्रकार के होते हैं - 1 अपर वैराग्य, 2. पर वैराग्य
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन विषयों के भोग को नाशवान, अनित्य और दुःख रूप समझकर उसके भोग से जो घृणा उत्पन्न हो जाती है और मन उनसे उदासीन होकर उसके विलास का त्याग कर देता है, उसे अपर वैराग्य कहते हैं। यह अपर वैराग्य भी दो प्रकार का होता है।
1. सोपाधिक,
2. निरुपाधिक
स्त्री, पुत्र, माता-पिता, घर-द्वार, अड़ोसी-पड़ोसी आदि की ओर से चित्त में जब विक्षेप होता है, तब व्यक्ति इनको त्यागकर चला जाता है। यह सोपाधिक वैराग्य है।
सन्त महात्माओं के सत्संग और अनन्त जन्मों के पूर्वार्जित पुण्य उदय होने पर जो विवेक बुद्धि द्वारा आत्मा, अनात्मा के विचार द्वारा घर-द्वार का त्याग कर देता है उसे निरुपाधिक वैराग्य कहते हैं।
निरुपाधिक वैराग्य सड़कर दुर्गन्धयुक्त नहीं होने पाता, परन्तु सोपाधिक वैराग्य की यदि उचित रक्षा नहीं हुई तो वह सड़कर दुर्गन्धयुक्त हो जाता है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस तरह वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सन्त महात्माओं ने वैराग्य की उपमा मक्खन से दी है। जैसे, ताजे मक्खन को जल्दी से जल्दी आग में तपाकर, उसमें से महमहाता हुआ ताजा घी तैयार कर लिया जाता है, जो स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्द्धक होता है, परन्तु यदि उसी मक्खन को दो-तीन दिन अथवा सप्ताहभर उसी तरह रहने दिया गया, आग में तपाकर घी तैयार न किया गया तो वह सड़ जायेगा। उसमें से दुर्गन्ध आने लगेगी, उसमें कीडे पड़ जायेंगे। इस तरह वह मक्खन फेंक देने लायक ही रहेगा। वह किसी काम का न रहा।
अब वैराग्य का दुर्गन्धित होना और कीडे पड़कर नष्ट होना क्या है, उसके लक्षण सुनो - कुटिया बना लेना, मंदिर आश्रम बनाना, चूल्हा-चक्की, मूसल-ढेकी आदि गृहस्थी की सामग्री रख लेना और फिर रुपया-पैसा जमा करना, इस तरह वह वैराग्यवान साधु गृहस्थ हो गया, यही मानो वैराग्यरूपी मक्खन का सड़कर दुर्गन्धित होना और उसमें कीड़े पड़ना है। इस मक्खन से अब ज्ञानरूपी घी नहीं निकल सकता। अनन्त जन्मों के पूर्वार्जित पुण्य के फलस्वरूप तो यह वैराग्य जागा और घर-द्वार, स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब परिवार सबका त्याग किया। इसके बाद जिस गृहस्थी का त्याग किया था, उसी गृहस्थी को रूप बदलकर फिर अपना लिया। इस तरह वह दीन का रहा, न दुनिया का। "धोबी का कुत्ता न घर का, न घाट का" हो गया।
निरुपाधिक वैराग्यवान को पहिले से ही विवेक रहता है। अतः, उसमें दृढ़ता रहती है, इसलिए उसका वैराग्य बिगड़ने नहीं पाता। उसके गिरने का भय नहीं रहता। ये दोनों वैराग्य बोध के पहिले होता है। अतः, इस बोध शून्य वैराग्यवान को सन्त महात्माओं तथा शास्त्रों की यही आज्ञा है कि वह संसार में न बिचरे, क्योंकि उसे विषयों के अस्तित्व का भान है। अतः संगदोष से उसे विषयों में पुनः आसक्ति हो सकती है। उसके गिरने का भय है। अतः, वह एकान्त में रहकर अपने वैराग्य को "खूष्ट न्याय" के समान पकायें। "खुष्ट न्याय" का मतलब यह होता है कि (खूष्ट कहते हैं-खूँटे को) जिस तरह खूँटे को जमीन में गाड़ते समय बार-बार ठोकर मारना और फिर हिलाकर उसकी मजबूती देखी जाती है, इसलिए कि जो भी पशु इसमें बाँधा जाये, वह कहीं उखाड़कर भाग न जाये। इसी प्रकार वह एकान्त सेवन, सत्पुरुषों का सत्संग और अध्यात्म शास्त्र वेदान्त का विचार करता रहे तथा अपने आत्मकल्याण, भगवत् दर्शन के लिए अपने हृदय में मछली के समान तड़प (जिज्ञासा) पैदा करे, इसी में उसका उद्धार है।
संसार में सोपाधिक वैराग्यवान तो बहुत मिलेंगे
"नारि मुई गृह सम्पति नासी, मूड़ मुड़ाइ होहि सन्यासी"
परन्तु, निरुपाधिक वैराग्य हजारों लाखों में किसी-किसी को होता है। विश्व के इतिहास में भगवान श्रीराम के समान वैराग्य न किसी को हुआ है और न किसी को होगा।
एक बार सोलह वर्ष की अवस्था में भगवान राम की इच्छा तीर्थाटन करने की हुई। राजा दशरथ को जब राम की इस इच्छा की जानकारी मिली तब उन्होंने उनके तीर्थ भ्रमण के लिए एक सुन्दर रथ सजवाया और आवश्यक व्यवस्था कर राज्य के कुछ कर्मचारी, सेवकों एवं राम के मित्रों के साथ उन्हें तीर्थ भ्रमण के लिए भेजा। राम अनेक तीर्थों में गए तथा पवित्र तीर्थों के भ्रमण के बाद वे अयोध्या लौट आये। तीथर्थों से लौटकर वापस आने के बाद उन्हें ऐसा प्रचण्ड वैराग्य हुआ कि न उन्हें भोजन में रुचि थी और न राजमहल के सुख भोग की ओर उनका ध्यान था। उसके नित्य की दिनचर्या में भी अन्तर हो गया। खाने-पीने, उठने-बैठने, सोने, हास-परिहास सबसे उन्हें अरुचि हो गई। वे दिन-रात या अमनस्क रहने लगे। राम की अवस्था कुछ ऐसी हो गयी कि खड़े हैं तो खड़े ही हैं, बैठे हैं तो बैठे ही हैं। न कुछ उत्सुकता है और न लालसा या कामना।
राजा दशरथ को जब राम की इस परिवर्तित दशा का हाल मालूम हुआ, तब वे बड़े चिंतित हुए। उन्होंने राम की दशा में परिवर्तन लाने के लिए अनेक प्रकार के भोग-विलास की सामग्रियों का राम के समक्ष आयोजन कराया। सुन्दर-सुन्दर षोडसी कुमारियों को अपने हाव-भाव एवं कटाक्षों से राम का हृदय परिवर्तित करने की आज्ञा मिली। इन सुन्दर कुमारियों ने राम के हृदय में परिवर्तन लाने के लिए अनेक युक्तियों से काम लिया, लेकिन वे असफल होकर लौट गयी। राम दिन-रात उदासीन वृत्ति में डूबे रहते थे। उनके मन में प्रचण्ड वैराग्य, पूर्ण रूप से घर कर गया था। तीर्थाटन का यही वास्तविक फल है और तीर्थ का यही महत्व है। तीर्थ करने के बाद यदि विषयों से परम वैराग्य और अन्तःकरण पवित्र न हो सका तो वह तीर्थाटन करना ही व्यर्थ है।
राम की इस दशा को देखकर सबको बड़ी चिंता हुई। इसी बीच अयोध्यानगरी में मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ। राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र का अपने दरबार में स्वागत किया और मुनि की चरण वन्दना करने के बाद राम की सोचनीय दशा का सम्पूर्ण वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया। यह सब सुनकर मुनि ने पहिले राम के निकट रहने वाले मित्रों को बुलाया और उनके द्वारा राम की दशा की जानकारी प्राप्त की। राम के मित्रों से मुनि को मालूम हुआ कि राम को न तो इस लोक के सुख भोग में आसक्ति है और न इन्द्र के स्वर्ग सुख की चाह है। उन्हें तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, जिसे पाकर और कुछ पाना बाकी न रहे। इस हाल को जानकर विश्वामित्र जी ने राम को राज दरबार में बुलवाया। राम दुर्बल, उदासीन एवं लड़खड़ाते हुए पैरों से चलते हुए राज दरबार में मुनि की आज्ञानुसार उपस्थित हुए। उन्होंने मुनि के चरणों की वन्दना की। तदुपरान्त, एक ओर हटकर खड़े हो गये, तब विश्वामित्रजी ने पूछा राम! तुम्हारी यह क्या दशा है? अपने मन की बात पूर्ण रूप से व्यक्त करो कि आखिर तुम चाहते क्या हो?
इस पर राम ने कहा भगवन्! मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो उस वस्तु की लालसा है, जिसे पाकर मनुष्य को फिर कुछ पाना बाकी न रहे। मैं देखता हूँ कि मनुष्य के लिए इस लोक और परलोक में सिवाय दुःख के कुछ सार नहीं है, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त दुःख ही दुःख में डूबा रहता है। इसे गर्भ में असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ता है। माता के उदर में, मल-मूत्र और दुर्गन्धयुक्त परिस्थिति में यह गर्भ का कष्ट सहता रहता है, फिर लघुद्वार से इसका जन्म होता है। इन कष्टों के बाद बाल्यावस्था में जब तक बोल नहीं सकता, शारीरिक विविध कष्टों में डूबा रहता है। पेट दर्द, सिर दर्द आदि कष्टों के आने पर न तो उसे बता सकता है और न उससे छूटने में समर्थ ही रहता है, सिवाय कष्टों को भोगते हुए रोते रहने के उसके पास कोई चारा नहीं होता। माता तथा उसके संरक्षक उसके कष्टों को समझ भी नहीं सकते। अतः, उन कष्टों के निवारण का कोई समुचित उपाय भी नहीं किया जा सकता। युवावस्था में इन्द्रियों के प्रबल होने पर वासनाओं से संबंधित अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है, फिर वृद्धावस्था तो सारे कष्टों का आगार ही है।
इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त मनुष्य को संसारमें कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। राम के मुँह से वैराग्य पूर्ण इस विवेचन को सुनते ही राज दरबार में बैठे हुए राजा दशरथ अपने आसन से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सम्पूर्ण राज दरबार में शोक का वातावरण व्याप्त हो गया। तब विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा- हे भगवन्! इस समय सम्पूर्ण विश्व में आपके समान परम पूज्यतत्त्ववेत्ता ज्ञान के भण्डार कोई नहीं है। आप राम के इन कष्टों के निवारणार्थ उन्हें उचित उपदेश देने की कृपा कीजिये। महर्षि विश्वामित्र के इस बात को सुनकर गुरु वशिष्ठ उठे। उन्होंने, गुरु होते हुए भी राम के चरणों की पुष्प पत्रादिकों से पूजा की। उनका हृदय प्रेम से गदगद् हो उठा। आकाश से देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि हुई और राज दरबार में ही श्रीराम को गुरु वशिष्ठ ने "योग वाशिष्ठ' महारामायण का ज्ञान दिया।
भैय्या! विमल वैराग्य का ऐसा स्वरूप होता है। बिना इस वैराग्य के ज्ञान सुलभ नहीं है और बिना ज्ञान के भगवान के चरणों में भक्ति नहीं हो सकती, जो सर्व दुःखों के नाशक और सुखों की खानि है।
अपर वैराग्य में विषयों के विलास का त्याग होता है, क्योंकि यहाँ बोध नहीं हुआ है, परन्तु पर वैराग्य में विषयों के अस्तित्व का ही त्याग हो जाता है। लकड़ी को डण्डा मानकर उससे घृणा करना यह 'अपर' और डण्डा है ही नहीं यह तो लकड़ी ही है, यह 'पर' वैराग्य है। अस्तित्व भगवान आत्मा को विषय मानकर उसका त्याग 'अपर और विषयों के अस्तित्व का ही त्याग 'पर' वैराग्य है।
कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ।।
यह पर वैराग्य है और
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब ब्रिषय बिलास ब्रिरागा ।।
यह अपर वैराग्य है। यहाँ तक वैराग्य है, आगे भक्ति का विवेचन है।
सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू ।।
मन, वचन और कर्म तीनों से, राम के पद में प्रेम होना यही सचा परमार्थ है।
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि अनूपा ।।
राम ब्रह्म है, परमार्थ रूप है। वे अजन्मा हैं, इन्द्रियों से परे आदि-अन्त से रहित और अनुपमेय है। उनके समान दूसरा कोई नहीं है।
सकल बिकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ।।
सनातन ब्रह्म राम विश्व की आत्मा है, 'मैं' है। वे समस्त विकारों और भेदों से रहित हैं। उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। देखो भेद तीन प्रकार के होते हैं -
1. सजातीय भेद -
मनुष्य एक जाति है, परन्तु इसमें स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक, युवा, वृद्ध हैं, ये सजातीय भेद हुए।
2. विजातीय भेद -
मनुष्य भेद हुआ। और पशु में भेद। ये दोनों अलग-अलग जाति के हैं। अतः, यह विजातीय
3. स्वगत भेद -
एक ही शरीर के अंगों का भेद, आँख, कान, नाक, मुँह, हाथ, पैर आदि का भेद स्वगत भेद है।
भगवान राम में इन तीनों भेदों का अत्यन्ताभाव है।
राम में सजातीय भेद नहीं है, किस तरह? देखो-राम की क्या जाति है?
राम सच्चिदानन्द दिनेसा ।।
राम, सत् है, चित् अर्थात् चेतन है और आनन्द स्वरूप है। सच्चिदानन्द है और जीव की जाति है।
ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन, अमल, सहज सुखरासी ।।
जीव अविनाशी है, अर्थात् सत् (सत्य) है। चेतन है और सहज सुखराशी अर्थात आनन्द स्वरूप है। इस तरह जीव और ईश्वर में सजातीय भेद बिलकुल नहीं है। यदि, जीव को राम ब्रह्म से भिन्न मानकर सत् मानोगे, तो ब्रह्म और जीव में सजातीय भेद आ जायगा। राम ब्रह्म से जीव को अलग मानकर यदि चेतन मानोगे तो सजातीय भेद आ जायगा और इसी तरह राम से भिन्न मानकर आनंद स्वरूप मानोगे तो सजातीय भेद आ जायगा इसलिए सत् है तो राम, चित् है तो राम, आनन्दस्वरूप है तो राम। अतः, जीव है ही नहीं वह राम ही है, क्योंकि इनमें भेद का अभाव है।
फिर समझो प्रश्न होता है कि सत् से भिन्न सत होता है या असत्? उत्तर होगा-असत्। चेतन से भिन्न चेतन होगा या जड़। उत्तर है- जड़ होगा और आनन्द से भिन्न आनन्द होगा या दुःख? उत्तर है, दुःख होगा। अब यदि हम राम ब्रह्म से जीव को सर्वथा भिन्न मानेंगे तो राम सत् है, चित् है, आनन्दस्वरूप है, तो जीव उससे भिन्न होने पर सत् से भिन्न असत्, चेतन से भिन्न जड़ और आनन्द से भिन्न दुःखरूप हुआ। इस तरह जीव असत्, जड़ और दुःखरूप हुआ। जब जीव असत् हुआ, तो असत् कहते हैं जो है ही नहीं उसे, बन्ध्यापुत्रवत्।
इसलिए, यदि जीव को भगवान राम से भिन्न मानोगे तो जीव का अस्तित्व ही खतम हो जायगा, वह रह ही नहीं सकेगा, इसलिए भाई! यदि जीव की रक्षा चाहते हो तो इस जीव बेचारे को राम ब्रह्म से अलग मत मानो। इसी में जीव का जीवन है। अलग होते ही वह मर जायगा। रहेगा कहाँ? अरे यार! सत्य दो नहीं होता, चेतन दो नहीं होता और आनन्द दो नहीं होता। अतः, ब्रह्म और जीव दोनों एक ही जाति के हैं। इसमें सजातीय भेद नहीं है।
एक जीव और दूसरा ब्रह्म यह भेद किसमें है? यदि यह भेद ब्रह्म में मानोगे तो वह भेद रूप हो गया, क्योंकि भेद तो दो में होता है, तो ब्रह्म या परमात्मा दो नहीं हो सकते और यदि अभिन्न है तो वह वही है, एक ही है, इस तरह भी भेद रहित सिद्ध हुआ।
अब विजातीय भेद पर समझो - अगर राम ब्रह्म से एक फूल को भी, एक तृण को भी अलग मानोगे तो उसमें विजातीय भेद आ जायगा। अतः, तिनका-तिनका, जर्रा जर्रा, कण-कण भगवान हैं।
'फूल है' इसमें 'फूल' विकल्प है या वस्तु ? उत्तर है-विकल्प है। तब विकल्प, तो अस्तित्वहीन होता है, अभावरूप।
शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः ।।
केवल शब्द भर सुनाई दे, परन्तु वस्तु का अभाव हो, उसे विकल्प कहते हैं। डण्डा सुनाई पड़ा, परन्तु ढूँढने पर डण्डा नहीं मिलेगा, लकड़ी ही लकड़ी हाथ में लगेगी। तब लकड़ी पर डण्डे का विकल्प हुआ। इसी तरह 'फूल' यह विकल्प किस पर हुआ? अस्तित्व 'है' पर हुआ। भास पर हुआ 'मैं' आत्मा पर हुआ, जो मन, वाणी से परे है, उस पर हुआ। जो भास है, अस्तित्व है, वह अस्ति, भाति, प्रिय है, सत् है, चित् है और आनन्दस्वरूप है, सच्चिदानन्द है। इस तरह राम ब्रह्म में विजातीय भेद का अभाव है। स्वगत भेद-जो पदार्थ व्यापक होता है, उसमें भेद नहीं हो सकता। भेद तो आकार-प्रकार में होता है। परिछिन्न में होता है, इसलिए राम ब्रह्म में स्वगत भेद का भी अभाव है।
'सकल बिकार रहित गत भेदा' का यही भाव है। वह अनूपा है, उपमा रहित है। उसके समान दूसरा कोई नहीं है, अनुपमेय है। इस तरह राम ब्रह्म में तीनों प्रकार के भेद का अभाव है। तब वह हुआ अभेदरूप और एक। क्योंकि, भेद तो दो में होता है। जब वह अभिन्न है, तब वह वही है, एक ही है। इसको कहते हैं परमार्थ। इसमें जो रत है, वे परमार्थी योगी हैं। जो एक है, वह अनुपमेय है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है, जो जैसा है, वह वैसा ही है। वह ऐसा, वैसा नहीं है।
देखो, यहाँ पर जितने तुम बैठे हो उनके रूप-रंग, आकार-प्रकार, सब एक- दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उसके समान दूसरा विश्व में कोई नहीं मिलेगा, जैसा उसकी आँख, कान, नाक, मुँह, चेहरा आदि वैसा दूसरा कोई नहीं है। वह जैसा है, वैसा ही है, जो है, वही है। वह अनुपमेय है, क्योंकि वह भगवान है, वह एक ही है। उसके समान कोई दूसरा नहीं है। इस अनुपमेयता से सब भगवान हैं।
प्रश्न है- स्वामी जी! जब सभी भगवान हैं, तब तो बहुत से भगवान हो गये। क्या कई भगवान हैं?
भैय्या! विषय को ध्यान से समझो -
एक कथावाचक किसी भावुक भक्त को रात भर रामायण सुनाते रहे, जब वह रामायण की कथा सुन चुका, तब वह भक्त कथावाचक से पूछने लगा कि पण्डित जी महाराज! आपने जो कथा सुनायी मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना और सब बातें समझ में आ गयी, केवल एक ही बात मेरी समझ में नहीं आयी, दयाकर उसी को समझा दीजिये।
पण्डित जी ने कहा- भाई! कौन-सी बात समझ में नहीं आई? पूछो। इस पर भक्त कहने लगा महाराज! ये जो आपने कथा कही उसमें राम राक्षस है या रावण राक्षस है, यही में समझ नहीं सका। इस पर पण्डित जी ने अपना सिर पीट लिया और अपने सारे परिश्रम पर पानी फिरा समझकर वे कहने लगे "भैय्या! न राम राक्षस है, न रावण राक्षस है। राक्षस तो हम-तुम दोनों हैं।"
इस तरह मत सुनो! देखो, विषय समझो - अरे यार! बहुत से भगवान नहीं हैं, जिसे तुम बहुत देख रहे हो, वह बहुत नहीं हैं, एक ही हैं। यहाँ पर विचार करना है कि जो अनेक है, वह एक ही है या अनेक? देखो इस पण्डाल में जो श्रोता बैठे हैं, उनकी गिनती करो। उनके सिर पर हाथ रख-रखकर गिनना आरम्भ करो-एक, आगे बढ़ो, अब दो, अब यहीं पर रुक जाओ और विचार करो कि जिसके सिर पर हाथ रखकर दो कह रहे हो वह क्या दो है? या एक ही है, जिसे दो कह रहे हो। आगे चलो 'तीन'। अब जिसके सिर पर हाथ रखे हो, वह तीन है या एक है। उत्तर मिलेगा- वह एक ही है। आगे चलो। चार, पाँच, छः इस तरह एक ही को तुम यह सब कहते चले आ रहे हो। वस्तुतः, वे है नहीं। सब एक ही हैं, जिसे तुम सौ, हजार, लाख करोड़ आदि कह रहे हो। यदि एक न हो तो सौ, हजार लाख की सिद्धि न हो। देखो-दो में से एक निकाल लो, दो नहीं रहा। तीन में से एक निकाल लो, तीन नहीं रहा। सौ में से एक निकाल लो, सौ नहीं रहा, सौ का अस्तित्व खतम, निन्यानबे ही रह गये। इसी तरह जिसमें से भी एक निकाल लोगे तो उसका अस्तित्व ही खतम। इससे सिद्ध हुआ कि यह जो अनेक कहा जा रहा है, वह एक ही है। एक वही है, जिससे भिन्न दूसरा न हो, यही एक की व्याख्या है।
मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म, मनुष्य के अनेक होने पर भी एक ही है। स्त्रियों का स्त्रीत्व धर्म, देवताओं का देवत्व धर्म, पशुओं का पशुत्व धर्म आदि। व्यक्तियों के अनेकत्व में भी एक ही है तो जो एक ही है वही राम है। इसका रहस्य किसानों से पूछो-गल्ले की राशि को जब किसान नापना प्रारंभ करता है, तब वह बड़े लहजे के साथ राशि नापना (गिनना) प्रारंभ करता है। वह एक को एक नहीं कहता। वह कहता है "रामे हे, रामे हे, रामे हे राम' इसके बाद वह दो कहता है। अतः, जो एक है, वह राम ही है।
ब्रह्माजी ने भगवान कृष्ण की स्तुति करते समय कहा कि भगवन! तुम एक हो।
एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः ।
नित्योऽक्षरोऽजस्र सुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः ।।
भगवान एक है-मन एक है, इसलिए वह भगवान है। चित्त एक है, इसलिए वह भगवान है, इन्द्रियाँ, आँख, कान, नाक, मुँह, हाथ-पैर आदि सब एक हैं। प्रश्न होता है-स्वामीजी! आँख, कान, हाथ, पैर आदि तो दो हैं, आपने इन्हें एक कैसे कहा? उत्तर है-अरे! यदि आँख दो हैं तो फिर दो काम उन्हें करना चाहिए, एक आँख देखने का काम करे और एक आँख सुनने का तब तो वे दो हैं, परन्तु जब वे केवल देखते ही हैं, अन्य कुछ नहीं तब सिद्ध है कि वह एक ही है। इसी तरह अन्य हो की संख्या की मान्यता को समझो, जब ये सब एक-एक ही हैं। शरीर एक, हड्डी एक, चमड़ा एक, रक्त एक। इस तरह सर्व एक ही एक है। इसलिए, सब भगवान ही है, क्योंकि भगवान एक है।
'मुक्ता' अपने आप में, भासै रूप अनेक ।
महाशंख लौ अंक ज्यों, बना आप ही एक ।।
यही अध्यात्म है, परमार्थ रूप भगवान है ।
भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल ।
करत-चरित घरि मनुज तनु, सुनत मिटहिं जग जाल ।।
वही कृपालु भगवान राम, भक्त, भूमि (पृथ्वी) ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएँ कर रहे हैं, जिसके सुनने से जगत् के सब जंजाल मिट जाते हैं।
सखा समुझि अस परिहरि मोहू, सिय रघुबीर चरन रत होहू ।।
इसलिए भैय्या निषाद! मोह को त्याग कर भगवान राम और सीता के चरणों में प्रेम करो। इसी में जीवन की सार्थकता है। तुम यह जो कुछ देख रहे हो, वह भगवान राम का चरित्र है और भगवान के चरित्र में दोष नहीं देखना चाहिए।
यही लक्ष्मण के द्वारा निषाद को ज्ञान-वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई मधुर वाणी कही गयी, जिसे सुनकर निषाद आनन्द विभोर हो उठा। बस, यही लक्ष्मण- गीता का उपसंहार है।
2. वाल्मीकि आश्रम
दोहा - सुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरषे राजिवनेन ।
सुनि रघुबर आगमनु मुनि, आगे आयउ लेन ।।
(124)
श्रीराम, लक्ष्मण और महारानी सीता जब गंगा पार करके चित्रकूट गये तो सबसे पहिले वे महर्षि बाल्मीकि जी के आश्रम में गये। वहाँ की पवित्रता और सुन्दरता को देखकर भगवान राम बड़े हर्षित हुए। उस समय महर्षि वाल्मीकि जी को जब पता चला कि भगवाम राम आ रहे हैं, तब वे उनकी अगुवानी करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने उनका अतिथि सत्कार किया।
मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा, आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा ।
देखि राम छबि नयन जुड़ाने, करि सनमानु आश्रमहिं आने ।।
भगवान राम ने मुनि को दण्डवत् किया। उनकी अलौकिक छबि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गये। उन्होंने बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया और सम्मानपूर्वक उन्हें अपने आश्रम में ले आये।
महर्षि वाल्मीकि जी को प्राणों के प्राण मंगलमूर्ति भगवान राम को अपने आश्रम में पाकर जो आनन्द हुआ उसकी सीमा नहीं थी। उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण सहित भगवान राम को सुन्दर आसन पर बिठाया और उनके लिए मधुर कन्द मूल और फल खाने के लिए मंगाये। जिन्हें उन्होंने बड़े प्रेम से खाया। वाल्मीकि जी श्रीराम के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देख-देखकर उनके मन में आनन्दका सागर उमड़ रहा है। तब भगवान राम महर्षि वाल्मीकि जी से अपने कमल सदृश्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन कहने लगे। हे मुनिराज ! हम आपसे अयोध्या से अपने यहाँ आने का क्या कारण बतावें, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल तो नित्य आपकी आँखों के सामने हैं। सम्पूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है।
हे प्रभो! पिता की आज्ञा का पालन, माता कैकई का हित, भरत जैसे धर्मात्मा भाई का राजा होना और आपके पवित्र कमल चरणों का दर्शन लाभ, यह सब मेरे परम सौभाग्य और पुण्य का प्रभाव है। हे मुनिनाथ! आपके श्रीचरणों के दर्शन से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गये, उनका हमें फल मिल गया। हम कृतकृत्य हो गये। भगवन! मेरे वन आगमन का कारण तो आपसे छिपा नहीं है। अतः, आप कृपा करके मेरे लिए किसी ऐसे स्थान में रहने का निर्देश कीजिये, जिससे मेरे कारण मुनियों के भजन-पूजन में किसी प्रकार की बाधा न हो, वे उद्विग्न न होने पावें, जहाँ पर मैं, लक्ष्मण और सीता सहित कुछ दिनों तक पत्तों और घास-फूस की कुटी बनाकर रहूँ।
सहज सरल सुनि रघुबर बानी। साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ।।
कस न कहहु अस रघुकुल केतू। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥
महर्षि वाल्मीकि जी भगवान राम के सरल, सहज और गूढ़ वचनों को सुनकर कहते हैं कि "श्रुति सेतु पालक" हे राम ! तुम धन्य हो, तुम ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि तुम श्रुति जो वेद है, सेतु अर्थात् उसकी जो मर्यादा है, उसके तुम पालक हो, रक्षक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो और महारानी जानकी साक्षात् त्रिगुणात्मिका माया है।
व्याकरण शास्त्र में 'राम' शब्द अकर्मक धातु है। इससे कर्त्तापन सिद्ध नहीं होता। यह अक्रिय होता है। 'रमुक' क्रीड़ायाम धातु से राम बनता है। यह आत्मनेपदी है। इसीलिए, राम सारे चराचर की आत्मा है, जो दिन-रात सबके अंदर से 'मैं' हूँ, 'मैं' हूँ कह रहा है। वही सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, चराचर का अस्तित्व सर्व की आत्मा, राम है। माता जानकी जी संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली त्रिगुणात्मिका माया है, मगर वे स्वतंत्र नहीं है। तुम्हारी सत्ता से चैतन्यता लेकर यह सब करती हैं, जैसे लोहा चुम्बक के कारण क्रियाशील होता है।
महाराज लक्ष्मण तो शेष के अवतार हैं और आप तो वस्तुतः जैसे हो, वैसे ही हो, जो हो, वही हो, जहाँ हो, वहीं हो। आपको क्या कहा जाये कि आप कैसे हो? मनुष्य रूप में देवताओं का काम बनाने के लिए तुमने अवतार धारण किया है।
देखो-अध्यात्म तत्त्व का निरूपण तीन प्रकार से होता है-
1. स्तुति के रूप में
2. गुरु शिष्य के संवाद के रूप में
3. उपदेश के रूप में
वेद स्तुति, गर्भ स्तुति, ब्रह्माजी द्वारा स्तुति, ये सब स्तुति के रूप में हुए। गीता में अर्जुन को गुरु शिष्य के सम्वाद के रूप में और भागवत में उद्धव को उपदेश के रूप में अध्यात्म कथन हुआ। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी स्तुति के रूप में आत्म तत्त्व का निरूपण कर रहे हैं।
विषय समझो - महर्षि ने जानकी को माया कहा। माया को सनातन ब्रह्म से यदि
भिन्न मानो तो माया नहीं, अभिन्न मानो तो माया नहीं। भिन्नाभिन्न मानो तो माया नहीं तो ऐसा कहो न कि स्वयं ब्रह्म ही है जो इस रूप में दिख रहा है। जो भगवान आत्मा है, उसकी यह देवी माया गुणमयी है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, यह ऐसी प्रबला है कि -
सिव चतुरानन देखि डेराहीं, अपर जीव केहि लेखे माँही।
सिव बिरंचि कहुँ मोहइ, को है बपुरा आन ।।
(उ.का. दो. 62-ख)
तो भैय्या! इससे तरने का तो केवल एक ही उपाय है और वह यह है कि जो मुझ आत्मा को जान लेता है, वह इससे बिन प्रयास तर जाता है। बात यह है कि आधार या अधिष्ठान के जान लेने पर माया का बाध हो जाता है। वस्तु तो ज्यों की त्यों रहती है, केवल दृष्टि बदल जाती है। डण्डा दिख रहा है, परन्तु ज्योंही यह जाना कि अरे! यह तो लकड़ी है, डण्डा, यह तो लकड़ी पर विकल्प हुआ है, जो है ही नहीं सब केवल लकड़ी है, इस बोध से वस्तु तो ज्यों की त्यों है, परन्तु अब लकड़ी ही दिखने लगी, डण्डा का अभाव हो गया। डण्डे का बोध हो गया।
किसी नगर में एक वैष्णव साधु रहता था। वह गणेशजी का बड़ा भक्त था। उसने पाँच तोले सोने की एक गणेश जी की मूर्ति बनवायी और पाँच ही तोले सोने के वजन की एक गणेशजी के वाहन मूसा (चूहे) की मूर्ति बनवायी और वह दोनों की बड़ी श्रद्धा से पूजा करने लगा। जब कुछ दिन बीत गये, तब दैव योग से उस साधु के पास एक पैसा भी न रहा। उसे जीवनयापन के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब उसने सोचा कि अभी इन दोनों मूर्तियों को बेचकर मिले हुए दामों से निर्वाह करें, फिर जब द्रव्य आ जायगा तब पुनः मूर्तियाँ बनवा ली जायेंगी। ऐसा सोच, वह उन मूर्तियों को लेकर एक सुनार के पास बेचने गया। सुनार ने दोनों को तौलकर दोनों का बराबर ही दाम लगाया और उसे दे दिया। दोनों के बराबर ही दाम देने पर वैष्णव साधु ने सुनार से कहा कि अरे भूतनी के! गणेशजी को मूसे के बराबर कर दिया। अरे! गणेश जी स्वामी हैं, मूसा वाहन है। क्या, कभी स्वामी और उसका वाहन बराबर हो सकता है? इस पर सुनार ने कहा- अरे बैरागडे! स्वामीपना और वाहनपना अर्थात् गणेशपना और मूसापना जो तुमने इन मूर्तियों में मान रखा है, उसे तुम निकालकर अपने पास रख लो। हमको तो सोने का दाम देना है। सोना तौल में दोनों का बराबर ही बराबर है। अतः, दाम भी बराबर ही बराबर दिया गया। ग्राहक की दृष्टि में आभूषण है, परन्तु सुनार या सर्राफ की दृष्टि में केवल सोना (अधिष्ठान) ही होता है। सुनार या सर्राफ की दृष्टि में आभूषण का बाध रहता है। आभूषण की तौल या कीमत नहीं होती, तौल और कीमत तो सोने की होती है। आभूषण माना गया है, सोना वास्तविक है। अस्तु, आभूषण है ही नहीं, सोना ही सोना है।
आत्मा की प्राप्ति के बाद प्रपंच का बाध हो जाता है। भास तो ज्यों का त्यों रहता है। केवल दृष्टि बदल जाती है। सर्राफ की दृष्टि में आभूषण तो ज्यों का त्यों रहता है, परन्तु दृष्टि सोने की रहती है। अधिष्ठान आत्म तत्त्व के बोध हो जाने पर माया अथवा जगत् प्रपंच का अर्थात् मान्यता का बाध हो जाता है। भास तो ज्यों का त्यों रहता है।
प्रश्न होता है- माया क्या है?
यह मैं हूँ, ये मेरा है, यह तू है, यह तेरा है। बस, यही माया है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है। शरीर तू है और शरीर तेरा है, यह माया है, यह कहाँ से कहाँ तक है?
गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानहु भाई ।।
गो माने इन्द्रिय, गोचर माने विषय (चारागाह) जहाँ तक इन्द्रियों का विषय है, वह सब माया है। मायापति ही एक ऐसा देश है, जहाँ इसका अत्यन्ताभाव है। शेष ब्रह्मलोक तक माया का सम्राज्य है।
महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि -
सो. - राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर ।।
अबिगत अकथ अपार नेति-नेति नित निगम कह ।।
(126)
महर्षि जी की यह स्तुति व्यापक अस्तित्व सत्ता भगवान राम की है। जिस सत्ता ने सामने खड़े हुए उस लीला विग्रह शरीर को धारण किया है, उसी सत्ता ने सारे चराचर को धारण किया है। यह स्तुति उसी अस्तित्व राम की हो रही है। यदि लीला विग्रह शरीर के लिए होता तो "वचन अगोचर" नहीं कहते, क्योंकि वह स्वरूप तो प्रत्यक्ष सामने खड़ा है, जो गोचर है। आँखों से दिखाई दे रहा है, उसके लिए तो वे "नीलाम्बुज श्यामल कोमलागं' ऐसा कहते हैं। अतः, यह स्तुति उस लीला विग्रह शरीर के साथ सारे चराचर को जो धारण किया हुआ है, उस अस्तित्व की हो रही है।
वे कहते हैं- हे राम! तुम्हारा 'स्व' का जो रूप है, वह इन्द्रियों और वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि वाणी उसी का कथन करती है, जिसका आकार-प्रकार होता है। उसी को मन जब मानता है, तब आँख देखती है, कान सुनता है, चित्त चिन्तन करता है, बुद्धि निश्चय करती है। तब कहीं वाणी उसी का कथन करती है। तब जब तुम्हारा स्वरुप 'स्व' माने स्वयं अर्थात् 'मैं' का ही रूप है, 'यावानहं' (जैसा 'मैं' हूँ) तब, जब तुम स्वयं, ऐसा 'मैं' हूँ, यह कहने में समर्थ नहीं हो, तब दूसरा, अर्थात मन, बुद्धि, वाणी तुम्हें कैसे कथन कर सकेगी, क्योंकि जो कुछ मैं कहूँगा, वह वाणी से ही तो कथन करूँगा। इसका अनुभव कर लो -
प्रश्न है- 'मैं' को कौन जान रहा है?
उत्तर- 'मैं' जान रहा हूँ।
क्या जान रहा हूँ? कि 'मैं' हूँ, यही न? जी हाँ।
तो ये सत्तापद हुआ अस्तित्व। इसका ज्ञाता अर्थात जानने वाला 'मैं' ही तो हूँ। इस सत्तापद में मुझ आत्मा अस्तित्व के सिवा देह, इन्द्रियाँ, मन, वाणी, बुद्धि ये है ही नहीं तो भाई! कौन कहेगा कि 'मैं' ऐसा हूँ इसलिए -
रामसरूप तुम्हार । बचन अगोचर बुद्धि पर ।।
अब 'स्व' के रूप में थोड़ी देर ठहर जाओ। अब यहाँ पर सिवा 'मैं' आत्मा, चैतन्यघनभूत अस्तित्व के किसी का भी पता नहीं।
हे राम ! (अस्तित्व, सत्ता, भगवान आत्मा 'मैं') तुम अविनाशी हो, अपार हो, कहाँ से कहाँ तक हो इसका पता नहीं। तुम व्यापक हो, अखण्ड हो, अपार हो, अद्वैत हो, अजर, अमर अविनाशी हो। बस, इतना ही कहकर वेद अर्थात् वाणी लौट आती है। (वेद वाणीरूप ही तो है)।
मान्यता जगत्, मन वाणी का विषय है और आत्म जगत्, मन, वाणी से परे 'आवागमनसगोचर' है। जिस आधार 'मैं' आत्मा भगवान ने कीट, पतंग से लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा सारे चराचर को धारण किया है, हे राम ! तुम्हारा वह स्वरूप 'वचन अगोचर बुद्धि पर' मन, बुद्धि, चित्त, वाणी आदि से परे है।
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि, हरि संभु नचावनिहारे ।
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा। औरु तुम्हहि को जाननिहारा ।।
जगत् तुम्हारा दृश्य है, तुम इसके द्रष्टा हो। उस जगत् प्रपंच के नचाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। वे भी जब तुम्हारे मर्म को नहीं जान सकते तब फिर दूसरों की क्या ताकत है, जो तुम्हें जान सकें।
तुम में देश, काल, वस्तु का अत्यन्ताभाव है, यही तुम्हारा मर्म है, जिसे ये भी नहीं जान सकते। प्रश्न है-तो क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनसे भिन्न हैं? उत्तर है- हाँ, क्योंकि-
उपजहिं जासु अंस ते नाना। विष्नु विरंचि सम्भु भगवाना ।।
जो अस्तित्व दूसरे शब्दों में 'मैं' उस लीला विग्रह शरीर राम का है अर्थात् उस शरीर को जिसने धारण किया है, उसी 'मैं' आत्मा ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शरीर को भी धारण किया है और वही 'मैं' आत्मा समस्त चराचर को धारण किया है, परन्तु यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इसलिए बड़प्पन दिया गया क्योंकि, ये ईश्वर कोटि के हैं।
जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से उपजते हैं, तब इनका अन्त भी होता है, ये मरते भी हैं। इस परिस्थिति में जो उपजहि और मरहि, वे जो न उपजते हैं और न मरते हैं, अर्थात् अजन्मा, अविनाशी, व्यापक ब्रह्म भगवान आत्माराम के मरम को कैसे जान सकते हैं। यही उसका मरम है। शास्त्रों में इसका प्रमाण आता कि -
चतुर्युग सहस्त्राणि दिनं पैतामहं भवेत् ।
पितामह सहस्त्राणि विष्णोश्च घटिका मता ।।
विष्णोर्द्वादश लक्षाणि, कलार्ध रौद्रमुच्यते ।
(दैवीमीमांसा भाष्य उत्पत्ति पादसूत्र-4)
चतुर्यग सहस्त्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते ।
पितामह सहस्त्राणिविष्णोरेको घटी मता ।।
विष्णोर्द्वादश लक्षाणि निमेषार्ध महेशितुः ।
दश कोट्यो महेशानां श्रीमातु स्त्रुटिरूपकाः।
(शक्ति रहस्य)
यारों युग जब एक हजार बार बीतते हैं तब ब्रह्माजी का एक दिन होता है। उसी माप से उनकी रात्रि, मास और वर्ष होते हैं। ब्रह्माजी के एक हजार दिन में भगवान विष्णु की एक घड़ी होती है अर्थात् भारतीय वर्तमान समय का चौबीस मिनट। भगवान विष्णु के बारह लाख दिन में भगवान शंकर का आधा पल होता है और भगवान शंकर के हजार पल में त्रिगुणात्मिका माया अर्थात् शक्ति का आधा पल होता है। अपने- अपने दिन के सौ-सौ वर्ष की आयु में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरे ब्रह्मा, दूसरे विष्णु, दूसरे शंकर की उत्पत्ति होती है।
प्रश्न होता है- ब्रह्मा, विष्णु, महेश होकर 'मैं' को जानेंगे या 'मैं' होकर 'मैं' को जानेंगे?
उत्तर है- 'मैं' होकर 'मैं' को जानेंगे।
बस, यही उसका मरम है। अपने 'मैं' को कुछ मानकर व्यक्ति, भगवान को ढूँढता है या 'मैं' को 'मैं' जानकर ढूँढता है? उत्तर मिलेगा 'मैं' को कुछ मानकर ढूँढ़ता है। प्रश्न - ढूँढता किसको है? उत्तर है 'मैं' को ही और पाता किसको है? 'मैं' को ही।
अरे! तो यही तो मरम है।
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा ।।
जब 'मैं' को ब्रह्मा मान लिया, विष्णु मान लिया, महेश मान लिया, तब इस मान्यता रूपी झाड़ी में 'मैं' छिप गया और इसी में भगवान आत्मा को ही जानना है। इसका ही दर्शन करना है, परन्तु 'मैं' रहकर, 'मैं' अमुक हूँ, ऐसा होकर नहीं, 'मैं' रहकर ही 'मैं' जाना जाता है। बस, यही मरम है।
सोई जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ।।
कौन जाने? सो। 'सो' किसके लिए आया है। उत्तर है- 'सो' अर्थात् 'मैं' जो जानेगा, क्योंकि 'मैं' अमुक हूँ, यह तो जानेगा नहीं। यदि, 'सो' शब्द को जानने वाले के लिए कहोगे तो अपने आपको कुछ मानकर जानने चलेगा तो उसे जानने का अधिकार नहीं है। वह नहीं जान सकता। अतः, 'सो' अब आ गया 'मैं' के लिए अर्थात् 'मैं' ही जनाता है और 'मैं' ही जानता है। बस, यही मरम है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश गोचर है। 'गो' माने इन्द्रिय, 'चर' माने विषय अर्थात् इन्द्रिय के विषय है और भगवान राम (आत्मा) अगोचर है अर्थात् इन्द्रियों से परे है, तो गोचर, अगोचर को कैसे जानेगा? जब तक कि वह भी 'अगोचर' न हो जाये। यही राम का मरम है। जानने की इच्छा गोचर की होती है और जब जानता है तब अगोचर होकर ही जानता है। गोचर रहकर नहीं जान सकता। भाई! अगोचर को ही अगोचर की प्राप्ति होती है। पुलिस को चोर पकड़ने की इच्छा होती है, मगर पकड़ता है, चोर होकर ही, पुलिस रहकर नहीं। पकड़ते समय वह यह नहीं जाना जा सकता कि यह पुलिस है। वह बिना ड्रेस का रहता है। वह चोर के साथ मिलकर चोरी भी करता है, जेल जाता है और उसके साथ-साथ मार भी खाता है। तब वह बड़े से बड़े केस को पकड़ पाता है। इस प्रसंग पर हृषीकेश की एक घटना याद आ गयी।
एक खूनी ग्यारह कत्ल कर चुका था। पुलिस उसे पकड़ सकने में असमर्थ रही। यह ग्यारह बार का कातिल गेरुवा वस्त्र पहिनकर महात्मा भेष में हृषीकेश में कुटी बनाकर रहने लगा था। एक सी. आई.डी. को उस पर सन्देह हो गया। वह उसके पास जिज्ञासु बनकर गया और उसका सेवक बनकर उसकी हर तरह सेवा करते हुए उसके साथ रहने लगा। एक दिन उस कातिल महात्मा के पास रात को चरस खत्म हो गया (वह चरस पिया करता था) उसने उस सेवक को आधी रात को आज्ञा दी कि जाकर शहर से चरस ले आ, जल्दी ला मुझे उसके बिना रहा नहीं जा सकेगा। जब उसके कई बार कहने पर भी वह शिष्य (सेवक) आधी रात को न जाकर, सुबह ला देने की बात कहता रहा और चरस लाने नहीं गया, तब वह बड़े क्रोध में आकर लाल-लाल आँखें दिखाकर उससे कहने लगा कि तू जानता है, मैं कौन हूँ? अपने जीवन में मैंने ग्यारह खून किये हैं, तू अभी जल्दी जाकर चरस ला नहीं तो तू बारहवाँ कत्ल होगा। तुझे जिन्दा नहीं छोडूंगा। बस, फिर क्या था। वह सेवक (सी.आई.डी.) गया और पास के पुलिस स्टेशन से पुलिस कर्मचारियों को ले आया और तुरन्त उसे गिरफ्तार कर लिया। भाई! जिसे पकड़ना है उसे वही रूप होकर पकड़ोगे तभी पकड़ सकोगे। भले ही तुम चाहे जन्म-जन्मान्तरतक जीव बने रहो, मगर जब भगवान को जानना चाहोगे तब भगवान ही होकर जान सकोगे, जीव रहकर नहीं।
देखो-तुम अपने घरमें टेरेलीन और विलायती कपड़े पहिनते हो, परन्तु यदि तुम भोपाल या दिल्ली मंत्री या राष्ट्रपति से मिलने जाओगे तो बढ़िया आंध्रप्रदेश की खादी की धोती, खादी का कुरता, जवाहर जाकिट, श्री नाट की बढ़िया खादी की टोपी, जेब में फाउन्टेन पेन, कलाई में घड़ी और हाथ में छड़ी लेकर सज-धजकर जाना पड़ेगा। इस तरह पं. जवाहरलाल नेहरु के छोटे भाई होकर ही राष्ट्रपति या मंत्री से मिल सकोगे अन्यथा नहीं। यह तुम्हारा नित्य का व्यवहारिक वेदान्त है।
जब तक अपने आपको कुछ मान रहे हो देह, जीव, ब्रह्म, वर्णी, आश्रमी, पंथ, मजहबवाला आदि तब राम को कैसे जानोगे? राम भी जब पंथ मजहब वाला हो, तब तो जान सकते हो, परन्तु वह तो कोई पंथ, आश्रम, मजहब वाला है नहीं। ईसा का कथन है, "नंगे ईसा के पास, नंगे होकर ही आना पड़ेगा।" मान्यता रुपी सारे कपड़े उतार फेंकना पड़ेगा तब वे मिल सकेंगे। यही मरम है। प्रश्न होता है- जानना क्या है और जानकर तुम्हीं हो जाना क्या है? यहाँ श्रुति आयी है।
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वान्नामरूपाद् विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।।
(मु.उ.खं. - 2, मं.-8)
जिस तरह नदियाँ समुद्र को जानने चलती हैं तो किनारे पर पहुँचकर वे अपने नाम और रूप का त्याग कर देती हैं। गंगा, यमुना, सिन्धु, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, शिवनाथ, तांदुला, खारुन आदि ये हुए नाम और प्रवाह हुआ रूप। समुद्र में मिलने के पहिले ये अपने नाम रूप का त्याग कर देती हैं तो हो गयी समुद्र। इसी तरह विद्वान विचारवान पुरुष जब नाम रूपात्मक अमुक भाव का त्याग कर दिया तो शुद्ध स्वरूप 'मैं' तत्त्व रह गया। यही परमात्मा की प्राप्ति है।
अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को ।
कि दाना खाक में मिलकर, गुले-गुलजार होता है ।।
नदियाँ समुद्र होकर ही समुद्र को जान सकती हैं, नदी रहकर नहीं। इसी तरह नाम रूप से अपने को अलग किया, तो रह गया शुद्ध चेतन आत्मा। जानने और जनाने का भाव तो तभी तक रहेगा, जब तक नदी और समुद्र दो रहेंगे। नदियाँ जब समुद्र में मिल गयी, तब फिर वे दो कहाँ? एक ही, हो गयी। इसी तरह भगवान को, भगवान होकर ही जाना जाता है। ब्रह्म ही, ब्रह्म को जानता है। अरे यार! सजातीय, सजातीय का मेल होता है। अतः, भगवान को जानने के लिए, तुम्हें भगवान होना पड़ेगा और भैय्या! होना क्या पड़ेगा, भगवान ही हो। अन्य कुछ नहीं, यही भगवान राम का मरम है।
इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्याः स्यन्दन्ते पश्चात्प्रतीच्यस्ताः
समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति समुद्र एव भवति ता यथा
तत्र न विदुरियमहमस्मीति...।।
(छान्दोग्य अ. 6, खण्ड 10वाँ)
परन्तु, बात यह है कि समुद्र में मिलने के बाद नदियों को यह याद नहीं रहता कि आज के पहिले में गंगा, यमुना, सिन्धु, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि थी, अब समुद्र हुई हूँ और यदि याद है तो फिर अभी मिली ही नहीं। अब जब नदी समुद्र हो गयी, नदी न रही, तब समुद्र भी न रहा, क्योंकि नदियों ने ही तो उसका 'समुद्र' नाम रखा था। जब नदी ही न रही, तब समुद्र कहेगा कौन?
अब जो रहा, वह न नदी है, न समुद्र है। उसी में दोनों कल्पित थे। इसी तरह यदि यह याद है कि आज के पहिले 'मैं' जीव था, अब ब्रह्म हुआ हूँ तो समझ लो कि अभी वह जीव ही है, क्योंकि जीव ने ही भगवान नाम रखा था। जब जीव ही न रहा तो भगवान कहेगा कौन? अब जो रहा, वह न भक्त है, न भगवान है। उसी में जीव, ब्रह्म, भगवान कल्पित है। भैय्या! गरमा-गरम मालपुवा खाओ, भाप निकल रही है, क्या करोगे गन्ना, गेहूँ बोकर।
खीजे दीन्हें अमर पद, रीझे दीन्हें लंक ।
अंधाधुन्ध दरबार है, मजा करो निश्शंक ।।
भगवान राम, रावण से खीझ गये अर्थात् बहुत नाराज हुए तो उनने, उन्हें देवताओं को भी दुर्लभ अमर पद प्रदान किया और विभीषण से रीझ गये अर्थात् बहुत खुश हुए तो उन्हें लंका का राज्य ही दे दिया। उनके रीझने और खीजने दोनों की सुन्दर गति है। ऐसा अंधाधुन्ध दरबार है वहाँ क्या कमी है? यह दरबार अंधाधुन्ध है, जहाँ तुम बैठे हो हरिद्वार, हृषिकेश, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, काशी आदि के लोग इस आनन्द से वंचित हैं, जिसको तुम लोग लूट रहे हो। इस अलौकिक ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, दण्डकारण्य है।
जानत तुम्हहि, तुम्हइ होइ जाई ।।
प्रश्न है - तुमको जानकर, तुम्हीं हो जाता है, इसका क्या प्रमाण है?
इसका यही प्रमाण है कि पा लेने के बाद वह अपना अनुभव बता नहीं सकता। इससे सिद्ध है कि जानकर वही हो गया।
ब्रह्मवित् ब्रह्मैवभवति ।।
ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाता है। अरे यार, जानने के पहिले भी वह वही रहता है। मान्यताओं को अपने 'मैं' पर आरोपित कर स्वयं उनसे ढँका था, जब उनका त्याग कर दिया तो रह गया 'मैं' आत्माराम ही। इस तरह जानने वाला राम, जनाने वाला राम और जिसको जाना वह राम। जब जानने के पहिले भी राम ही है, तब जाना किसको? किसी को नहीं। जाना कौन? किसी ने नहीं और जनाया किसने ? किसी ने नहीं। न कुछ जाना, न कुछ जनाया, न कुछ जानने की चीज रही। यही राम का मरम है। केनोपनिषद की श्रुति आयी है -
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ।।
( 72/3 )
जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को जाना है और जो कहता है कि उसे नहीं जानता हूँ तो इन दोनों ने उसे नहीं जाना, क्योंकि ब्रह्म इनसे भिन्न कब है, जिसे ये जानेंगे। जानना दो में होता है, एक में नहीं। जब एक ही है तब कौन किसको जानेगा? यही राम का मरम है।
भले भयो हरि बीसरो, सिर से टली बलाय ।
जैसे थे वैसे रहे, अब कछु कहा न जाय ।।
महात्मा उग्रानन्द जी महाराज मस्ती में आकर ऐसा कहा करते थे।
तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनन्दन। जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥
महर्षि जी कहते हैं कि हे राम! वे ही भक्त तुम्हें जान सकते हैं, जिनका हृदय चन्दन के समान शीतल और पवित्र हो। तुम्हारी कृपा अर्थात् बिना आत्मकृपा के तुम्हारा अर्थात् आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुंस्वाम् ।।
(मुण्डकोपनिषद 3/2/3)
भाव यह है कि यह आत्मा प्रवचन द्वारा, श्रवण द्वारा प्राप्त नहीं होता। जिज्ञासु का हृदय जब आत्मदर्शन के लिए मछली के समान तड़पता है अथवा व्याकुल होता है, तब तत्काल ही भगवान आत्मा सर्व का 'मैं' अपना स्वरूप प्रगट कर देता है।
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥
(मुण्डकोपनिषद् 3/2 / )
बलहीन पुरुष को आत्मानुभव कभी नहीं होता। बल शब्द से यहाँ जिज्ञासा बल समझना चाहिए। आत्म जिज्ञासा को ही आत्म कृपा भी कहते हैं, क्योंकि किसी और ने बाँधा हो तो कोई खोले, जबकि अपने संकल्प से स्वयं ही बंधा है, तब अपने आप ही छूट भी सकता है। न तो इसके लिए सत्य में कोई बन्धन है, न मोक्ष।
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे वृहन्ते तस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ।
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥
( श्वे.उ.1/6)
अर्थात् सर्व के प्रेरक भगवान को अपने आपसे भिन्न मानकर अनादिकाल से हंस जीव, ब्रह्म चक्र याने संसार में भ्रमता रहता है और जब भगवान और अपने आप 'मैं' को शरीर से भिन्न करके एकता का अनुभव करता है, तब वह तत्काल ही समस्त बन्धनों से मुक्त होकर अमृतत्व पद (कैवल्य पद) को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि जितनी उपाधियाँ हैं, माया के ढक्कन में ही हैं। ढक्कन उठाते ही केवल 'मैं' का 'मैं' ही रह जाता है। श्रुति के इस कथन से यही सिद्ध होता है कि जीव का आवागमन इत्यादि भगवान से अपने आप 'मैं' को अलग मानने में ही है।
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ।।
(मुण्डकोपनिषद् 8)
उस परावर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर इस जीव की हृदय ग्रन्थि छूट जाती है। सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। इसके सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं और आवागमन के चक्र से छूट जाता है। भगवान राम कहते हैं कि -
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा ।।
इससे सिद्ध होता है कि जीव का सहज स्वरूप जीव नहीं। उसका सहज अर्थात् स्वाभाविक स्वरूप भगवान 'आत्मा' ही है। जीव तो कृत्रिम अर्थात् माना हुआ स्वरूप है।
श्री मानसकार ने विनय में कहा है कि -
जिव जबतें हरितें विलगान्यो। तबतें देह गेह निज जान्यो ।
मायाबस स्वरूप बिसरायो। तेहि भ्रमते दारुन दुःख पायो ।।
(वि.प. 136)
बचपन में गुरुजी ने स्कूल में पढ़ाया कि बेटा! देखो पुरुष लीन होते हैं। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
अन्य पुरुष 'वह' है, मध्यम पुरुष 'तू' है और उत्तम पुरुष 'मैं' है। 'मैं' उत्तम पुरुष है, इसे भूलना नहीं। इस तरह गुरुजी ने तो 'मैं' को उत्तम पुरुष बताया और चेला जी ने 'मैं' को अधम पुरुष मान लिया अर्थात् 'मैं' को देह मान लिया। 'मैं' देह हूँ मान लिया। देह, अधम ही तो है। प्रमाण लो -
छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा ।।
शरीर अधम है। मल मूत्र का भांड है। सदा अपवित्र है, यह उत्तम नहीं है, पर क्या करते हो चेला जी ने 'मैं' को अधम मान लिया। उत्तम पुरुष भगवान आत्मा 'मैं' ही है, जिसे गुरुजी ने बचपन में पढाया है। अब उत्तम को पुरुष के बाजू में लगा दो, अब हो गया 'पुरुष उत्तम' अर्थात् 'पुरुषोत्तम' भगवान आत्मा 'राम'।
चिदानंद मय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी ।।
भगवान के तीन रूप हैं।
आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। जो भासे (भास) यह भगवान का आधिभौतिक रूप है। जो प्रगटै (राम, कृष्ण) यह आधिदैविक रूप है और जो न भासै, न प्रगटै यह आध्यात्मिक रूप है। भगवान का आधिभौतिक रूप ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारा चराचर है। इसमें कर्मकाण्डी को संसार का भ्रम होता है। यह मोह है।
भगवान का आधिदैविक रूप राम और कृष्ण का लीला विग्रह शरीर है। इसमें उपासक को नर का भ्रम होता है। यह भ्रम कागभुसुण्डी, गरुड़, ब्रह्मा और सती को हुआ था। यह महामोह है।
महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहि न बेगि कहे खग मोरें ।।
और भगवान का आध्यात्मिक रूप जो न भासता है, न प्रगट होता है 'मैं' आत्मा है। ज्ञानी को इसमें जीव का भ्रम होता है। यह आत्म सम्मोह है।
महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवन्! ये जो तुम्हारा लीला विग्रह शरीर है, वह चिदानन्द मय है।
सच्चिदानन्द क्यों नहीं कहा? अरे । यही तो मरम है। महर्षि जी चिदानन्द उस अस्तित्व 'है' के लिए कह रहे हैं, जिस 'है' अस्तित्व ने उस लीला विग्रह शरीर को, जो उनके समक्ष खड़े हैं, धारण किया है, क्योंकि -
इच्छामय नर वेष सँवारे। होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥
अरे भाई! चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सारा चराचर चिदान्दस्वरूप है। यह भगवान भास ही तो है। गजेन्द्र ने भगवान भासकी स्तुति की थी।
ॐ नमो भगवते तस्मैयतएतच्चिदात्मकम् ।
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ।।
(भाग. स्क.-8 अ.-3, श्लोक-2)
यह जो सारा चराचर जो विकल्परहित अवस्था में भास रहा है, उस भगवान भास को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या विलक्षण प्रसंग है, परन्तु इसको वही समझेगा जो -
तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत-भगत उर चंदन ।।
चिदानंदमय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी ।।
यह लीला विग्रह शरीर भी चिदानन्दमय है। अस्ति, भाँति, प्रिय ही तो है। अस्ति माने 'है' अस्तित्व सत् ही तो है, जो महर्षि जी के सम्मुख खड़े हैं, जो भास रहे हैं और यदि प्रिय न हो तो भक्त लोग आराधना क्यों करें। इसलिए 'चिदानन्द मग देह तुम्हारी' कहा। जिनके सब विकार नष्ट हो चुके हैं, वे ही इसे समझ सकते हैं। देखो - विकार क्या है? अपने स्वरूप भगवान आत्मा 'मैं' को 'मैं' न जानकर, कुछ न कुछ मानना देह मानना, जीव मानना, ब्रह्म मानना आदि यही विकार है। देह मानकर स्त्री, पुरुष, वर्णी, आश्रमी, पन्थी, मजहबी मानना, फिर जीव मानकर स्वर्गी, नरकी, पुण्यी, पापी आदि मानना और ब्रह्म मानकर दृष्टा, साक्षी, व्यापक, अखण्ड, निरंजन, निराकार आदि मानना ये ही सब विकार हैं। ये सब विकार जिनके नष्ट हो चुके हैं और जो अपने शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा को 'मैं' का 'मैं' ही जानता है, वह ही तुम्हें जान सकता है, क्योंकि वह भी चिदानन्द स्वरूप है।
नर तनु घरेहु संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ।।
ऐसे जो आप हैं, वे सन्त और देवताओं के कार्य के लिए इस लीलाविग्रह शरीर को आपने धारण किया है और आप लौकिक राजाओं की सी लीला कर रहे हैं। परन्तु, वह आप नहीं हैं।
जथा अनेक बेष धरि, नृत्य करइ नटकोइ ।
सोइ-सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ।।
(उ.का. दो.-72 ख)
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ।
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ।।
हे राम! तुम्हारे चरित्र को देखकर जड़ अर्थात् अविवेकी जिन्हें स्व-स्वरूप आत्मा का बोध नहीं है, वे मोहित हो जाते हैं, अर्थात् भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि संसार का प्रवेश दो इन्द्रियों के द्वारा हृदय देश में होता है। देखकर और सुनकर श्रीराम के चरित्र को संसार क्यों कहा?
झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें।
जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन भ्रम जाई ।।
जो तीन काल में न हो, उसे चरित्र कहते हैं। तो फिर भासता क्यों है? अरे! यही तो भगवान राम की लीला है। लीला को देखकर जिनको मोह (भ्रम) होता है, वे जड़ हैं, दानव हैं, मानव हैं। क्योंकि, मानसकार ने कहा कि -
असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥
रज्जू (रस्सी) में सर्प का भ्रम होगा, जब रज्जू का अज्ञान होगा और भ्रम किसको नहीं हुआ? गरुड़ को हुआ, सती को हुआ, भुसुन्डी को हुआ, ब्रह्मा को हुआ, नारदको हुआ।
गरुड़ को भ्रम हुआ -
भव बंधन ते छूटहिं, नर जपि जाकर नाम ।
खर्ब निसाचर बाँधेउ, नागपास सोइ राम ।।
(उ.कां.दो. 58)
जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार के बन्धन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बाँध लिया। क्या वे भगवान हैं? सती को देखो -
जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरहँ मति भोरि ।
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ।।
(बा.का. दो. 108)
जिनका 'मैं' यह चरित्र देख रही हूँ, क्या वह ब्रह्म है?
भुसुन्डी को देखो -
प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह ।
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद सन्दोह ।।
(उ.का. दो. 77 ख)
भाई! बहुत मुश्किल है। लीला देखो तो राम जाता है और राम देखते हो तो लीला या चरित्र जाता है। अब जो चीज पसंद हो चुन लो। अरे! सर्प देखते हो तो, रज्जू नहीं और यदि रज्जू देखते हो तब सर्प नहीं। चरित्र को देखकर बुध अर्थात् विवेकीजन सुखी होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्व-स्वरूप भगवान आत्मा में न कुछ हुआ है, न कुछ हो रहा है और न कुछ होने वाला है।
नटकृत बिकट कपट खगराया। नट सेवकहिं न ब्यापइ माया ।
सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला। जा पर होइ सो नट अनुकूला ।।
बस, इसीलिए बोधवान सुखी होते हैं।
दोहा- पूँछेहु मोहि कि रहौं कहें, मैं पूछत सकुचाउँ ।
जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखावों ठाऊँ ||127||
हे राम। तुमने मुझसे पर्णशाला बनाकर रहने के लिए स्थान पूछा है, परन्तु भगवन्! मैं आपसे पूछते सकुचाता हूँ। आप ही बता दो कि जहाँ आप नहीं हो 'मैं' वहीं आपको रहने के लिए स्थान दिखाऊँ।
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मन महुँ मुसकाने ।।
महर्षि वाल्मीकि जी के प्रेमरस से सने हुए इन गूढ वचनों को सुनकर भगवान राम सकुचकर मुस्करा दिये, क्योंकि 'मैं' आत्मा राम कहाँ नहीं है, क्या नहीं है और किसका नहीं है?
बालमीकि हँसि कहहिं बहोरी। बानी मधुर अमिअ रस बोरी ।।
फिर महर्षि जी हँसकर राम से अमृतमय मीठी वाणी में कहने लगे कि भगवन्! सरकारी आज्ञा हुई है, इसलिए आपके रहने के लिए मैं स्थान बतलाता हूँ। जहाँ आप निवास कीजिये। मैंने छोटे-बड़े चौदह प्लाट चुने हैं, उनमें बहुत से ऐसे हैं, जो अकेले रहने लायक हैं। कुछ ऐसे हैं, जहाँ आप और सीता जी दोनों रह सकते हैं और कुछ ऐसे हैं, जहाँ आप सीता और लक्ष्मण सहित तीनों रह सकते हैं। तो, पहला स्थान सुनिये-
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ।
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ।।
जिनके कान समुद्र के समान हैं और तुम्हारी कथा नदियों के समान है, जैसे समुद्र में कितनी भी नदियाँ आकर मिलती जायें, परन्तु समुद्र अघाता नहीं, उसमें बाढ़ नहीं आती। उसी प्रकार तुम्हारे जन तुम्हारी कितनी ही कथा जीवन पर्यन्त निरन्तर सुनते रहें, परन्तु वे अघाते नहीं अर्थात् तृप्त नहीं होते। उनका वह हृदय, आपके निवास के लिए सुन्दर घर है। वहाँ आप निवास कीजिये।
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं दरस जलघर अभिलाषे ।
निदरहिं सरित सिन्धु सर भारी । रूप बिंदु जल होहिं सुखारी।
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक। बसहु बन्धु सिय सह रघुनायक ।।
आपके श्रीमुख के दर्शन के लिए जिनके नेत्र चातक हैं, जो आपके दर्शनरूपी मेघ की ही आशा में जीते हैं, जिन्हें लोक लोकान्तर में सिवा आपके किसी की भी अपेक्षा नहीं है, उनके हृदय में आप लक्ष्मण और सीता सहित निवास कीजिये। यह बड़ा प्लाट है।
दोहा - जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनि जीहा जासु ।
मुकताहल गुन गन चुनइ, राम बसहु हिय तासु || 128||
जिनका हृदय मानसरोवर के समान है, जिह्वा हंसिनि है, तुम्हारा गुणानुवाद मोती है, तब जिस हृदय रूपी मानसरोवर में, जिह्वा रूपी हंसिनी, तुम्हारे गुणानुवाद रूपी मोती को चुगती रहती है। उसके हृदय में आप निवास कीजिये, यह छोटा प्लाट है। यहाँ आप अकेले रह सकते हैं।
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा । सादर जासु लहइ नित नासा ।
तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पट भूषन घरहीं ।।
जिसकी नासिका, आपके पवित्र और सुगन्धित सुन्दर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है और जो आपके, अर्पण करके भोजन करते हैं और प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं।
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी ।
कर नित करहिं राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहि दूजा ॥
जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर, बड़ी नम्रता के साथ, प्रेम सहित झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं।
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ।।
और जिनके चरण आपके दर्शन के लिए चलने का परिश्रम करते हैं, हे राम! आप उनके मन में निवास कीजिये।
मंत्र राजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ।
तरपन होम करहिं बिधि नाना । बिप्र जेवाँइ देहिं बहु दाना ।
तुम्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भायें सेवहिं सनमानी ।।
दोहा- सबु करि माँगहि एक फलु राम चरन रति होउ ।
तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ || 128||
उपरोक्त सम्पूर्ण साधनों का फल, जो केवल यही चाहते हैं कि भगवन! हमारा आपके (राम के) चरणों में विमल प्रेम हो, ऐसी भक्ति हमें दीजिये, उनके मन मंदिर में माता सीता सहित आप निवास कीजिये।
काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ।
जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया। तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया ।।
काम, क्रोध, मद, अभिमान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग और द्वेष, दम्भ, कपट और मोह से जिसका हृदय रहित हो। हे राम ! उनके हृदय में निवास कीजिये। भैय्या! बिना आत्मबोध के यह संभव नहीं है।
सब के प्रिय सब के हितकारी। सुख दुख सरिस प्रसंसा गारी ।
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी ।।
तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माँही ।।
जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाला है, जिनको सुख-दुःख, प्रशंसा और गारी एक समान हैं, जो विचारकर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं और जो जागते-सोते सब समय आप ही के शरण में हैं। सिवा आपके, जिनकी दूसरी गति नहीं है, हे राम! उनके मन मंदिर में आप निवास कीजिये।
जननी सम जानहिं परनारी । घनु पराव बिष तें बिष भारी ।
जे हरषहिं पर संपति देखी। दुखित होहिं पर विपति विसेषी ।
जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पिआरे। तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ।।
जो परायी स्त्री को अपनी माता के समान जानते हैं, दूसरे के धन को विष के समान समझते हैं, जो दूसरे की सम्पत्ति को देखकर हर्षित होते और विपत्ति को देखकर दुखित होते है, जिन्हें तुम प्राणों से प्रिय हो, हे राम ! उनका हृदय ही तुम्हारे रहने के लिए सुन्दर निवास स्थान है। वहाँ निवास कीजिये।
दोहा- स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात ।
मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भ्रात ।।130।।
हे राम! जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ तुम्हीं हो, उनके हृदय मंदिर में तुम लक्ष्मण और सीता सहित निवास करो।
अवगुन तजि सबके गुन गहहीं । बिप्र घेनु हित संकट सहहीं ।
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ।।
जो अवगुणों को छोड़कर, सबके गुणों को ही ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए जो नित्य संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत् में मर्यादा है, उनका सुन्दर मन आपके निवास करने का स्थान है।
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ।
राम भगत प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर बसहु सहित बैदेही ।।
जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसको सब तरह से तुम्हारा ही भरोसा है, जिनको तुम्हारी भक्ति ही प्रिय है, हे राम ! उनके हृदय मंदिर में सीता सहित आप निवास करें।
जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥
सब तजि तुम्हहिं रहइ उर लाई। तेहिके हृदय रहहु रघुराई ।।
जाति, पाँति, धन, धर्म, बड़ाई, प्रिय परिवार और सुख देने वाले घर सबको छोड़कर, जो केवल आपको ही हृदय में धारण किये रहता है, हे रघुनाथ जी! आप उनके हृदय में निवास कीजिये।
सरगु, नरकु, अपबरगु समाना। जहँ तहँ देख घरें धनु बाना।
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा ।।
स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान हैं, क्योंकि वह सर्वत्र आप ही को देखता है और जो मन, वचन, कर्म से आपका दास है, है राम! उनके हृदय में डेरा कीजिये।
जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ।
बसहु निरन्तर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥131||
जिसका हृदय सर्व कामनाओं से रहित है, जिसे मोक्ष की भी कामना नहीं है और जिसका आपके चरणों में स्वभाविक सहज स्नेह है। सहज सनेह उसे कहते हैं, जिसमें बनावटी न हो, जैसे पिता-पुत्र का सनेह, सहज सनेह है, वहाँ पर विधि- निषेध नहीं रहता। जो मोक्ष को भी ठुकराता है, अरे! मोक्ष है क्या चीज? क्योंकि, बन्ध-मोक्ष तो जीव देश की चीजें हैं, अज्ञान देश के हैं। परन्तु, भैय्या! एक बात है, बोध के पश्चात् ही भगवान राम के प्रति सहज सनेह होता है। अज्ञानी हृदय कभी निष्कामी नहीं होता और भगवान राम निष्काम है। कोई निष्काम को पाकर ही तो निष्काम होगा। ऐसा जिसका हृदय है, भगवन! वहाँ आप निवास कीजिये। इस तरह महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के लिए चौदह स्थान बतलाया -
एहि बिधि मुनिबर भवन देखाए । बचन सप्रेम राम मन भाए ।
कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक । आश्रम कहउँ समय सुखदायक ।
चित्रकूट गिरि करहु निवासू । तहँ तुम्हार सब भाँति सुपासू ।
सैलु सुहावन कानन चारू । करि केहरि मृग बिहग बिहारू ।।
फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा- हे प्रभो! अब मैं इस समय जहाँ आश्रम बनाकर रहना चाहिए वह स्थान आपको बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिये। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। वह सुहावना पर्वत है और सुन्दर वन है, जो हाथियों, हिरणों एवं सिंहों और पक्षियों का विहार स्थल है।
नदी पुनीत पुरान बखानी । अत्रिप्रिया निज तप बल आनी ।
सुरसरि धार नाउँ मन्दाकिनी। जो सब पातक पोतक डाकिनी ।।
अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं। करहिं जोग जप तप तन कसहिं ।
चलहु सफल श्रम सबकर करहू । राम देहु गौरव गिरिबरहू ।।
वहाँ पवित्र नदी है, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूइया जी अपने तपोबल से लायी थी, वह गंगा की धारा है। उसका नाम मन्दाकिनी है, वह सम्पूर्ण पापरूपी बालकों को खा डालने के लिए डाइन रूप है।
अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम ! आप वहाँ जाकर, सबके परिश्रम को सफल कीजिये और चित्रकूट को गौरव दीजिये।
दोहा - चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ ।
आइ नहाए सरित बर, सिय समेत दोउ भाइ ।। 132।।
बस! यहीं पर वाल्मीकि आश्रम का उपसंहार है।
3. चित्रकूट दरबार
आत्म जिज्ञासुओं !
जब भगवान श्रीराम के वियोग में महाराज दशरथने प्राण त्याग कर दिया, तब कैकय देश से महात्मा भरत और शत्रुघ्न अयोध्या से दूत भेजकर बुलाये गये, भरत ने अयोध्या में आते ही सम्पूर्ण स्थितियों का अनुभव किया तो उन्हें महान दुःख हुआ। इन असह्य वेदनाओं से पीडित, महात्मा भरत की दशा का वर्णन नहीं हो सकता। पिता की मृत्यु सुनते ही उनकी दशा करुण हो गयी।
सुनत भरतु भए बिबस बिषादा। जनु सहमेउ करि के हरि नादा ।।
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल ब्याकुल भारी ।।
इसके बाद जब उनने भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का वनगमन सुना तो-
दोहा- भरतहिं बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु ।
हेतु अपनउ जानि जियँ थकित रहे घरि मौनु ||160||
इसके बाद माताओं, गुरुजनों और परिजनों के सहित भरत शोक सागर में डूबने लगे, उनकी दयनीय दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रसंग में माता कौशल्या ने स्नेहपूर्वक उन्हें अनेक प्रकार से धीरज बँधाया और राम के वन से आते तक उन्हें राज-काज संभालने के लिए आग्रह किया। गुरु वशिष्ठ ने भी उन्हें अनेक प्रकार से सांत्वना देते हुए समझाया कि बेटा भरत -
दोहा - सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ ।
हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ।। 17 1।।
इसलिए माता-पिता की आज्ञा को स्वीकार कर राज्य का कार्य भार संभालो, यही उचित है, तब महात्मा भरत अत्यंत दुःख और वेदना से भरे हुए कहते हैं।
दोहा - ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार।
तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ||180||
जैसे कोई ग्रह पीड़ा से पीड़ित, बात रोग का रोगी हो, उसे बिच्छु का डंक लग जाये, इसके बाद उसे मदिरा पिला दी जाये, तो उसकी जो दशा होगी, वही दशा मेरी है।
कैकेई, रूपी ग्रह से मैं ग्रसित हूँ, पिता का निधन हो गया है यह मुझे बात रोग है, भगवान राम चौदह वर्ष के लिए वन चले गये हैं, यह मुझे बिच्छु का डंक लगा है। इसके बाद भी मुझे जो राज सिंहासन पर बैठने की सलाह दी जा रही है, यह मुझे मदिरा पिलाने के समान है। क्योंकि, राजमद मदिरा का ही रूप है।
प्रभुता पाय काह मद नाहीं
अतः, मैंने अपने मन में एक ही निश्चय किया है, वह यह है कि - -
दोहा- आपनि दारुन दीनता कहउँ सबहि सिरु नाइ ।
देखें बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ ||182||
आन उपाउ मोहि नहिं सूझा । को जिय कै रघुबर बिनु बूझा।
एकहिं आँक इहइ मन माहीं । प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाहीं ।
जद्यपि मैं अनभल अपराधी । भै मोहि कारन सकल उपाधी ।
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी। छमि सब करिहहि कृपा बिसेषी ।।
भरत के इस निश्चय को सुनकर सब आनन्द विभोर हो गये, सबने महात्मा भरत की भूरि-भूरि प्रशंसा की। माताएँ, मंत्रीजन, गुरु और नगर के प्रजाजन सबों ने मुक्तकंठ से कहा कि महात्मा भरत, राम प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति ही है। अंत में सबको लेकर महात्मा भरत भगवान राम के पास चित्रकूट चले, साथ ही चतुरंगिनी सेना थी, घोड़े, हाथी, रथ और पैदल जिसमें रहते हैं, उसको चतुरंगिनी सेना कहते हैं।
मातृ मंडल, मंत्रिमंडल, ब्राह्मण मंडल, प्रजा मंडल और गुरु वशिष्ठ इन सबके सहित महात्मा भरत भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे। महात्मा भरद्वाज जी ने जब इन्हें देखा तब वे सोचने लगे कि इतनी बड़ी सेना का किस तरह स्वागत किया जाय, वे ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही सुन्दर-सुन्दर कन्याओं के रूप में उनके समक्ष ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ प्रगट हुई और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहने लगी कि महाराज! हम सब सेवा में उपस्थित हैं, कृपाकर हमें आज्ञा दीजिये कि हम कौन- कौन सी सेवा करें।
अणिमा - जो अणु के समान छोटा हो जाये।
महिमा - जो चन्द्रलोक तक चला जाये।
गरिमा- जो पहाड़ की नाई वजनीय हो जाये।
लधिमा - जो अत्यन्त हल्का हो जाये।
प्रकाम्य-जो इच्छा करो, वही हो जाये।
वशीत्व - जिसको चाहे, अपने वश में कर ले।
ईशीत्व - शासन करने वाला, आदि। इस तरह आठ सिद्धियाँ और नव निधियाँ हैं, इन्हें अधिक जानकर क्या करोगे-इन सबको महात्मा भरद्वाज जी बोले, इनकी पहुनई करना है, जितना हो सके इनकी खूब सेवा करो। बस, फिर क्या था इनके प्रताप से भरत समाज के प्रत्येक के पास एक-एक कल्पवृक्ष, कामधेनु और अमूल्य रत्न चिन्तामणि आदि सब हो गये। बड़े-बड़े महल बन गये, देवलोक से रम्भा, मेनका, उर्वशी आदि अप्सरायें इनकी सेवा में आ-आकर जुट गयी और उन्हें हर तरह की सुख-सुविधा प्रदान करने लगीं, परन्तु मानसकार यहाँ चित्र खींचते हैं कि-
दोहा - संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार ।
तेहि निसि आश्रम पिंजराँ राखे भा भिनुसार ।।215||
चकवा और चकवी रात्रि में अलग-अलग रहते हैं, रात्रि में इनका मिलाप होता ही नहीं, यह ईश्वरीय विधान है। सम्पत्ति चकवी है, भरत जी चकवा हैं और मुनि की आज्ञा ही खेलाने वाला है, इन सब ऐश्वर्यों का प्रभाव अयोध्या से आये हुए सब पर तो पड़ा, परन्तु भरत इनसे बिल्कुल ही अछूते रहे।
जैसे, किसी बहेलिये के द्वारा एक ही पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात्रि में संयोग नहीं होता, उसी प्रकार भोग सामग्री चकवी और भरत चकवा इन दोनों को मुनि ने आश्रम रूपी एक ही पिंजड़ा में रात भर रखा, परन्तु महात्मा भरत ने मन से ही उनका स्पर्श तक नहीं किया। वे रात भर भगवान राम के लिए तड़पते रहे, उन्हें नींद न आयी और इसी तरह सबेरा हो गया। सबेरा होने पर उन्होंने समाज सहित तीर्थराज में स्नान किया, फिर मुनि भरद्वाज को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद ले, चित्रकूट की ओर चले। चित्रकूट पहुँचने पर वहाँ चार सभाएँ हुई। पहिली सभा महात्मा भरत की गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुई, दूसरी सभा भगवान राम की, तीसरी सभा महाराज जनक की और चौथी सभा रानियों की हुई। इसे सन्त समाज में चित्रकूट का दरबार कहते हैं, यहाँ का विषय बड़ा ही क्लिष्ट है। यहाँ ज्ञान, वैराग्य की धार बहती है, यहाँ कौन क्या कह रहा है, इसे हर एक की बुद्धि नहीं समझ सकती। चलो, अब प्रसंग पर आयें -
दोहा - निसि न नींद नहिं भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच ।
नीच कीच बिच मगन जस मीनहिं सलिल सँकोच ।।252।।
चित्रकूट पहुँचकर अयोध्यावासी, जिनको जहाँ भी जगह मिली, रात्रि को विश्राम करने लगे सब सो गये, परन्तु भरत की दशा कुछ और ही थी, उन्हें रात भर नींद नहीं आयी, उनके मन में अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प होते रहे।
कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली ।
केहि बिधि होइ राम अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाउ न एकू ।
अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी।
मातु कहेहुँ बहुरहिं रघुराऊ । राम जननि हठ करबि कि काऊ ॥
राम, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अवश्य अयोध्या लौट सकते हैं, परन्तु गुरुदेव भी राम की रुचि जानकर ही कहेंगे, माता कौशल्या के कहने पर भी वे यहाँ से लौट सकते हैं, परन्तु माता क्यों हठ करने लगेगी।
मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँ कुसमउ बाम बिधाता ।
जौं हठ करउँ त निपट कुकरमू। हरगिरि ते गुरु सेवक धरमू ।।
मैं तो और भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सेवक का धर्म तो हरगिरि अर्थात् शिवजी के कैलास से भी अधिक भारी होता है। सेवक यदि अपने स्वार्थ के लिए स्वामी से हठ करता है तो वह सेवक का धर्म नहीं है।
एकउ जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भरतहिं रैनि बिहानी ।
इस तरह सोचते-सोचते रात बीत गयी, परन्तु एक भी राक्ति मन में निश्चित न हो सकी। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्रीराम जी को । सर नवाकर बैठे ही थे कि गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें अपने पास बुलवा भेजा -
दोहा - गुरु पद कमल प्रनामु करि बैठे आयसु पाइ ।
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ।।253।।
भरत जी गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गये, मंत्रिमंडल ऋषियो का मंडल, प्रजा मंडल और महिला मंडल सब आ-आकर गुरुदेव को प्रणाम कर आज्ञा पा यथा स्थान बैठते गये। इस सभा के सभापति भगवान वशिष्ठ हुए, इनकी सभा चातुरी देखो-इन्होंने सोचा कि सबसे पहिले मुझे यहाँ राम की महिमा बताना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर कैकई का कोई पक्षपाती बैठा होगा तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इस तरह सभा में राम के विरोधियों का पता लग जायेगा, इस अभिप्राय से उन्होंने भगवान राम की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया।
बोले मुनिबरू समय समाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना ।
धरम धुरीन भानुकुल भानू । राजा रामु स्वबस भगवानू ।
सत्यसंध पालक श्रुति सेतू । राम जनमु जग मंगल हेतू ।
गुर पितु मातु बचन अनुसारी। खल दलु दलन देव हितकारी ।
नीति प्रीति परमारथ स्वास्थु । कोउ न राम सम जान जथारथु ।।
राजनीति किसको कहते हैं, समाज में बड़ों के सामने किस प्रकार बोलना चाहिए और अपना मनोभाव (स्वार्थ) रखकर, किस प्रकार वहाँ से अपने को अलग कर लेना चाहिए, इनको जानना हो तो चित्रकूट के चारों दरबार का मनन करना चाहिए।
गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे सभासदगणों! पहिले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि राम कौन हैं? उन्हें पहले समझ लो।
भगवान राम धर्म के धुरीण और सूर्यवंश के सूर्य हैं, राजा हैं और भगवान हैं।
अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि राजा तो प्रजा के वश में होता है, स्वतंत्र नहीं होता तो यहाँ स्ववश क्यों कहा? उत्तर है कि भगवान हैं इसलिए स्ववश हैं। अरे भाई! जन जीव राजा है, तब तो प्रजावश है और जब भगवान राजा है, तो स्ववश भगवान् हैं। श्रीराम सत्य नैष्ठिक हैं, सत्यवादी हैं, श्रुति जो वेद है उसका सेतु अर्थात् मर्यादा के रक्षक हैं और संसार को सुख देने वाले हैं, गुरु, पिता-माँ, की आज्ञा के पालक हैं। खल दलों के नाशक हैं, देवताओं के हितकारी हैं और फिर नीति, प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ को राम के समान यथार्थ रूप में जानने वाला विश्व में कोई दूसरा नहीं है। यह हम नहीं कहते कि कोई जानते ही नहीं, जानते होंगे, परन्तु यथार्थ रूप से जानने वाले विश्व में उनके सिवा अन्य नहीं है।
बिधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ।
अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ।
करि बिचार जिर्यं देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबही के ।।
सूर्य, चन्द्रमा, दिक्पाल, लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी कर्म, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल, माया, जीव, राजे-महाराजे तथा सारे चराचर में राम की आज्ञा शिरोधार्य है। बिना श्रीराम की आज्ञा के एक पत्ता भी नहीं हिलता, परन्तु यह कब जान पड़ेगा? इसका अनुभव उसी को होगा, जिसका हृदय नीके होगा। "करि बिचार जिर्यं देखहु नीके" यह मलिन हृदय से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यदि मलिन हृदय को यह अनुभव हो जाय तो फिर वह अनैतिक कार्य न करे। यों तो सभी जानते हैं कि बिना राम की आज्ञा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर लोग ऐसा कहते भर हैं, मानते भर हैं, जानते नहीं। तब जो नीका है, उसी का हृदय नीका होगा, तो भैय्या! नीक तो राम के सिवा कोई नहीं, जीव हृदय कभी नीक हो नहीं सकता, यह निर्विवाद अटल सिद्धान्त है। लोग कहते जरूर हैं कि भगवान के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए, परन्तु जीव हृदय कभी निष्काम नहीं हो सकता। निष्काम तो केवल एक राम ही है।
राम की आज्ञा सारे चराचर को शिरोधार्य है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण तो यही है कि पहिले तुम राम हो जाओ, फिर तो बताना नहीं पड़ेगा, स्वयं अनुभव हो जायेगा। किसी के प्रताप, महिमा, स्वरूप और चरित्र को यदि यथार्थ रूप से जानना है तो पहिले वही हो जाओ, इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपना स्वरूप जो 'मैं' आत्मा है (शरीर दृष्टि को छोड़कर) उसे भगवान राम जानो, राम अनुभव करो, उस समय तुम्हारा हृदय नीक होगा और तभी इसका तुम्हें अनुभव होगा कि 'राम रजाइ शीस सब ही के है।' हाँ, सुनकर, पढ़कर भले जान लो, परन्तु बिना अनुभव के नहीं जान सकते।
जब श्रीराम ऐसे हैं तब - -
दोहा- राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ ।
समुझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ ।।254।।
गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जब सारे चराचर पर राम की आज्ञा शिरोधार्य है, तब उनकी आज्ञा का ही पालन करना, हमारा परम कर्त्तव्य है। इस तरह पहिले वे सब कुछ कह गये, अब पैंतरा बदलते हैं, वे कहते हैं अरे! मैं यह नहीं कहता कि यही करो, बड़े-बड़े बुद्धिमान सयाने, ऋषि मंडल, मंत्रिमंडल, प्रजा मंडल, महिला मंडल सब बैठे हो, सबकी राय में जो ठीक ऊँचे वही करो। जो वास्तविक है, उसे हम कह चुके। यही सभाचातुरी है कि अपनी सम्पूर्ण बातें कहकर फिर वहाँ से अलग हो गये और उन्हीं पर छोड़ दिया। यही राजनीति है, भाई! सूर्यकूल के आचार्य हैं, ऐसे वैसे तो है नहीं। कैसे बुढऊ ने सबको बाँध लिया, जिनकी व्यापक दृष्टि है उन्हें और जिनकी शरीर दृष्टि है उन्हें भी। श्रीराम की आज्ञा सभी पर है, विषय समझो -
जो जिसका अस्तित्व, आधार और कारण होता है, उसके बिना वह टस से मस नहीं हो सकता, यही आज्ञा है, यही उसके ऊपर उसकी आज्ञा शिरोधार्य है। हाँ, जीव की आज्ञा किसी पर होती है, किसी पर नहीं होती, क्योंकि जीव परिछिन्न होता है, परन्तु भगवान राम की आज्ञा सारे चराचर तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त, सबके ऊपर है, क्योंकि वह सारे चराचर का अस्तित्व है। आधार है, कारण है, उसमें व्यापक है, वही है। जो सबमें रमा हो, जिससे कोई देश, काल, वस्तु खाली न हो, उसी का नाम है, राम। वह कल्याण स्वरूप होने से शिव है।
नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ।।
(कठोपनिषद (2/12)
जो अस्तीति 'है' है, वही अस्तीति आत्मा सबमें नित्य 'मैं' हूँ, 'मैं' हूँ कह रहा है, उसे प्राप्त करने और कहाँ अन्यत्र जाओगे? फूल है, ब्रह्मा है, जीव है, ईश्वर है, जड़ है, चेतन है, ज्ञान है, अज्ञान है, जगत् है, ब्रह्म है आदि। एक तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त ऐसा कोई है, जो 'है' से खाली हो, जिसमें 'है' न हो। इसी व्यापक सत्ता का नाम राम है, यह सत्ता है, अस्तित्व है, वजूद है। तो भाई! जिसके बिना जो है ही नहीं, तभी तो उसकी आज्ञा उस पर शिरोधार्य है, यही सत्ता अस्तित्व ही भगवान राम है, आत्मा है, 'मैं' है। यह लबालब भरा हुआ है, जो पापी और पुण्यात्मा सबमें है। एक बार दिल्ली में हमसे एक सज्जन ने पूछा-स्वामी जी, जब ईश्वर सबमें व्यापक है, तब वह पापी में भी होगा?
हमने कहा- भाई! होगा नहीं, है।
इस पर वह कहने लगा कि आज तरह-तरह के अनाचार, अत्याचार, दगाबाजी रिश्वतखोरी, मिलावट, चोरी और व्यभिचार आदि बुरे काम सर्वत्र हो रहे हैं और उन पाप कर्म करने वालों में जब भगवान है, तब वह भगवान इन बुरे काम करने वालों को रोकता क्यों नहीं? हमने कहा वह रोकता तो है, याररा! पर, वह कुकर्मी मानता है नहीं। इस पर वह कहने लगा, कैसे रोकता है? हमने कहा देखो, झूठ बोलना पाप है, यह बात सत्य है, न। उसने उत्तर दिया-जी हाँ! तब हमने कहा- जो झूठ बोल रहा है, उसको यह ज्ञान है या नहीं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वह झूठ है। उसने उत्तर दिया-जी हाँ, उसे यह ज्ञान है। हमने कहा-तब, यह ज्ञान किसका है? ईश्वर का है या उस पापी का? उत्तर मिला- ईश्वर का है। हमने कहा-भैय्या! तो और कैसे रोकेगा? क्या लाठी लेकर आयेगा, खोपड़ी फोडने।
कोई भी शराबी, जुआरी, दुराचारी, चोर जब इन कामों को करने जाता है, तब भीतर से उसको ज्ञान रहता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, वह पाप है। यह विवेक उसे रहता है। यह विवेक उस पापी का नहीं, ईश्वर का है। जो इस विवेक का आदर करता है, वह बच जाता है और जो इस विवेक का अनादर करता है, नहीं मानता उसे दण्ड भोगना पड़ता है। कोई-कोई कहते भी हैं कि क्या करें यार! मैं इस काम को नहीं करना चाहता था, मेरे भीतर से कोई कह रहा था कि तू इस काम को मत कर, परन्तु मैं उसे नहीं माना और मित्रों के चक्कर में आकर यह कार्य कर डाला, जिसके कारण यह विपत्ति आयी। भीतरवाला ऐसा न्यायाधीश है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। वहाँ रिश्वतखोरी, पक्षपात आदि कुछ नहीं चलता यही तो "राम रजाइ शीस सबही के" है। तब, जब नीके हिय से विचार करता है तब वह राम की आज्ञा का पालन करता है और जिसका हृदय नीके नहीं है, वह उसकी आज्ञा को भंग करता है और अनेक विपत्तियों में पड़ता है।
उमा दारु जोषित की नाई, सबहिं नचावत राम गोसाईं ।।
कठपुतलियों का नाच रात में होता है। उन्हें नचाने वाला पर्दे के भीतर रहता है, वह सबको देखता है, पुतलियों को भी और दर्शकों को भी। उसे कोई नहीं देख पाता। स्वयं पुतलियों में नाचने की शक्ति नहीं है। वे नचाने वाले के द्वारा नचायी जा रही है।
इन्द्रियाँ कठपुतलियाँ हैं 'मैं' आत्मा राम इन्हें नचाता है, वह मान्यता रूपी पर्ने के भीतर है, वह सबको देखता है, उसे सब अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, इन्द्रियाँ आदि कोई नहीं देख पाता, ये कठपुतलियाँ, अज्ञान के अंधेरे में नाच रही हैं, ज्ञान के प्रकाश में इन्हें देखो तो वे न तो नाच रही हैं और न कोई उन्हें नचा रहा है। यह जीव हृदय से नहीं जाना जा सकता, यह तो नीके हिय से ही जाना जा सकेगा। अशुद्धि काल तक तो उसका नाम जीव है और जब शुद्ध हो गया तब वह राम ही है।
अब प्रसंग पर आ जाओ -
गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि भैय्या! सबका सुख इसी में है कि श्रीराम का राज्याभिषेक हो जाये, इसलिए ऐसा उपाय करो जिससे श्रीराम चित्रकूट से अयोध्यापुरी लौट जायें। गुरु वशिष्ठ के इस कथन का सभी ने स्वागत किया, क्योंकि उनके श्रीमुठ से नीति, परमार्थ और स्वार्थ से सनी हुई वाणी निकली।
सब सादर सुनि मुनिबर बानी। नय परमारथ स्वास्थ सानी ।।
नीति, परमार्थ और स्वार्थ की वाणी कौन-सी है समझो -
दोहा- राखें राम रजाइ रुछ। हम सबकर हित होइ ।
समुझि सयाने करहु अब । सब मिलि संमत सोइ ।।254।।
यह नीति की वाणी है।
बिधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला से लेकर राम रजाइ सीस सबही के
तक परमार्थ की वाणी है।
सब कहुँ सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मग एकू ।।
केहि बिधि अवध चलहिं रघुराऊ। कहहु समुझि सोई करिअ उपाऊ ।।
ये स्वार्थ से सनी हुई वाणी है।
धरम, धुरीन, भानुकुल भानू से लेकर कोउ न राम सम जान यथारथु
तक राजाराम की महिमा है।
बिधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला से लेकर जोग सिद्धि निगमागम गाई ।।
तक भगवान राम की महिमा है।
उतरु न आव लोग भए भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ।।
गुरु वशिष्ठ की इस वाणी को सुनकर सारी सभा शांत हो गयी, सब चुपचाप बैठे रहे। किसी को कोई उत्तर नहीं सूझा तब महात्मा भरत बड़े विनीत भाव से नम्रतापूर्वक गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और सिर नवाकर बोले। वे कहने लगे- गुरुदेव!
भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक ते एक बड़ेरे ।।
जनम हेतु सब कहँ पितु माता। करम सुभासुभ देइ बिधाता ।।
हमारे इस सूर्यकुल में एक से एक बड़े-बड़े राजा हुए, जो योद्धा, तपस्वी, ऊर्ध्वरेता, विश्व विजेता, आत्म नैष्ठिक हुए। जन्म के कारण तो माता-पिता हैं, परन्तु शुभाशुभ कर्मों के फल का देने वाला तो विधाता ही है।
दलि दुख सजइ सकल कल्याना। अस असीस राउरि जगु जाना ।
सो गोसाइँ बिधि गति जेहिं छेकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी ॥
इस वंश पर सदैव आपकी दया और कृपा की छत्रछाया रही, आपकी आशीष ही एक ऐसी है, जो सम्पूर्ण क्लेशों को नष्ट करके हर तरह के कल्याणों से सजा देने वाली है। आपकी महिमा के प्रताप को तथा चमत्कार को सारा विश्व जानता है, आप विधाता की गति को भी छेकने वाले हैं, उनकी रेख में मेख मारने वाले हैं, आपने जो टेक, टेक दी, जो निश्चय कर लिया उसे टाल सकने की शक्ति संसार में किसी की नहीं है।
दोहा- बूझिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु ।
सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु ।।255।।
ऐसे गुरुदेव सब प्रकार से समर्थ होते हुए मुझसे जो उपाय पूछ रहे हैं तो भरत इसे अपना दुर्भाग्य ही समझता है। इस तरह जब महात्मा भरत ने हजारों वर्ष पहिले के इतिहास की याद दिलायी तो भरत की इस गुरु निष्ठा को देखकर गुरुदेव के हृदय में अनुराग उमड़ पड़ा, वे गद्गद हो गये और बोले-कि बेटा भरत! तुमने जो कहा, सब सत्य है। गुरुदेव वशिष्ठ ने विधाता की गति को कहाँ पर छेका था, उस इतिहास को सुनो -
सूर्यवंश में दशरथ के पहिले स्वयंभू मनु से लेकर इक्ष्वाकु तक जितने राजा हुए उन सबके एक-एक पुत्र थे, दशरथ के ही चार पुत्र हुए। इसी कुल में दिलीप हुआ है।
वशिष्ठ जी ब्रह्माजी के मानस पुत्र में से हैं, उन्होंने अपने पिता ब्रह्माजी से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। मुझे संसार में कौन-सा काम करना है? तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि तुम अयोध्या में जाकर सूर्यवंश में पुरोहिताई करो, क्योंकि आगे चलकर इस वंश में भगवान राम का जन्म होने वाला है। वहाँ तुम उनके कुलगुरु होकर संसार में पूजनीय होगे। पिता ब्रह्मा की आज्ञा को शिरोधार्य कर, वे अयोध्या में आकर पुरोहिताई करने लगे थे।
इसी कुल में राजकुमार दिलीप का जो अपने पिता का इकलौता पुत्र था, विवाह हो रहा था। जब विवाह मण्डप में भाँवरें पड़ रही थीं तब राजकुमार दिलीप जो वर के रूप में विवाह मंडप में बैठे थे, एक भयानक मूर्ति को अपने सामने खड़े देखकर घबराकर गुरुदेव वशिष्ठ (जो कि वहाँ उपस्थित थे) से कहने लगे, गुरुदेव! यह कौन भयानक मूर्ति काल के सदृश्य सामने खड़ी है। मुझे उसे देखकर भय लग रहा है। वशिष्ठ ने योगबल से उसे देखा। वह सचमुच यमराज था, जो दिलीप के प्राण ले जाने के लिए वहाँ उपस्थित हुआ था। वशिष्ठ जी ने तुरन्त यमराज के सामने ब्रह्म रेखा खींच दी और मंडप में विवाह कार्य कराने वाले पुरोहित को कहा कि अभी कुछ देर के लिए भाँवर का कार्य रोककर शेष कार्य आप सम्पन्न कराइये। मैं थोडी देर में आता हूँ. मेरे वापस आने पर वह कार्य पूरा किया जायेगा। ऐसा कहकर, वे तुरन्त योगबल से ब्रह्माजी के पास ब्रह्मलोक पहुँच गये और ब्रह्माजी से कहने लगे-आपने मुझसे कहा था कि उस कुल में भगवान राम का जन्म होने वाला है, परन्तु उस वंश का इकलौता राजकुमार दिलीप जिसका विवाह हो रहा है, उसकी मृत्यु होने वाली है। उसके प्राण लेने यमराज सामने खड़ा है।
इसकी मृत्यु के बाद वह कुल समाप्त हो जाने वाला है, यह क्या बात है? और आपने ब्रह्मा होकर ऐसा असत्य भाषण क्यों किया ? इस पर ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सचमुच सातवें भाँवर पड़ते ही विवाह मंडप में ही दिलीप की मृत्यु लिखी हुई है, तब उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि जो कुछ हो रहा है, वह मेरे लेख के अनुसार ही हो रहा है। तब वशिष्ठ कहने लगे कि जब ऐसा ही था तब आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा? आज जब वह वंश समाप्त हो जायेगा तब वहाँ भगवान राम का जन्म किस तरह होगा? मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। आप अपने उस लेख को काटिये। इस पर ब्रह्माजी ने कहा कि भाई मेरा लिखा अमिट होता है। वह लिख जाने के बाद न तो स्वयं मुझसे ही काटा जा सकता है और न भगवान में ही ऐसी सामर्थ्य है कि उसे वह काट दे, हाँ तुम संत हो, गुरु हो। संत और गुरु विधाता और भगवान से भी बड़ा होता है, तुम चाहो तो उस लेख को काट सकते हो। तुममें वह शक्ति गुरु और संत होने के नाते है। ब्रह्माजी की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने तुरन्त ब्रह्मा जी के उस लेख पर स्याही फेर दी अर्थात् उसे काट दिया और फिर विवाह मंडप में उपस्थित होकर शेष कार्य पूरा कराया।
इस तरह उनने अपने शिष्य को ब्रह्मा के लेख को काटकर काल के गाल से बचा लिया और यमराज को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो कानून के दायरे में रहते हैं, परन्तु संत महापुरुषों के लिए कोई कानून की पाबंदी नहीं होती। इसी राजा दिलीप को अपनी रानी समेत पुत्र प्राप्ति की कामना से, इन्हीं के (वशिष्ठ) आश्रम में जाकर इनकी गाय कामधेनु की पुत्री नन्दिनी की 21 दिनों तक सेवा करनी पड़ी थी, जिसके वरदान के फलस्वरूप उस कुल में राजा रघु का जन्म हुआ था। राजा दशरथ को भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गुरु वशिष्ठ की ही शरण लेनी पड़ी थी।
इन्हीं सब बातों को बताकर महात्मा भरत गुरुदेव की शक्ति और इस कुल पर उनकी सदैव कृपा दृष्टि रहने का चित्र खींच रहे हैं। भरत की गुरु भक्तिपूर्ण बातें सुनकर गुरुदेव ने कहा -
तात बात फुरि राम कृपाहीं । राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥
बेटा भरत! तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है - राम से विमुख होने पर स्वप्न में भी किसी की सिद्धि नहीं हो सकती।
प्रश्न होता है कि राम के सन्मुख (सम्मुख) होना और विमुख होना क्या है?
उत्तर है - मानना विमुख होना है और जानना सन्मुख (सम्मुख) होना है।
लकड़ी यदि अपने को डण्डा मानती है तो यही उसका लकड़ी से विमुख होना है और यदि अपने को लकड़ी जानती है, तो यही उसका सन्मुख (सम्मुख) होना है। इसी तरह अपने 'मैं' आत्मा को कुछ भी मानना यही भगवान आत्मा 'मैं' से विमुख होना है और जब मानना छोड़ दिया, सर्व मान्यताओं का त्याग कर दिया तो 'मैं' का 'मैं' रह गया। यह मुझ आत्मा राम के सन्मुख होना है।
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ।।
अनन्त जन्मों की अनन्त मान्यताएँ हैं। अतः, अनन्त पाप हैं। भगवान इन सब पापों के तत्काल नाश का कितना सरल और सुगम उपाय बता रहे हैं कि जीव ज्यों ही सन्मुख हुआ कि तुरन्त उसके सब पाप नष्ट हो गये? यह सरकारी विधान है, जो अटल है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि –
सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥
(गीता अ.-18, श्लोक-66)
सर्व धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, फिर मैं सर्व पापों से तुझे छुड़ा लूंगा।
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा ।।
मुझ आत्मा भगवान के दर्शन का यही अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अमुक भाव जीव का कृत्रिम स्वरूप है और 'मैं' आमा हूँ, यह उसका सहज स्वरूप है। डण्डा, लकड़ी का कृत्रिम स्वरूप है और लकड़ी इसका सहज स्वरूप है। गुरुदेव कहते हैं -
सकुचउँ तात कहत एक बाता । अरघ तजहिं बुध सरबस जाता ॥
हे तात, मैं एक बात बड़े संकोच के साथ कह रहा हूँ। वह यह कि बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर, आधा छोड़ दिया करते हैं। विश्व की आत्मा राम सर्वस्व हैं, जो सर्व का सर्व है, सुख का सुख है। जिसके बिना जिसका अस्तित्व ही न रहे, वही उसका सर्वस्व होता है। लकड़ी डण्डे का सर्वस्व है। यह पिता अर्थात् रक्षक है, माता अर्थात् जन्म देने वाली है। आधार है, कारण है, उसमें व्यापक है। इसी तरह भगवान राम विश्व के सर्वस्व हैं।
देखो - भगवान राम के जन्म के बाद महाराज दशरथ के आँगन में दर्शकों की भीड़ लग गयी। उन दर्शकों में नगर के नर-नारी, बड़े-बड़े ऋषि, मुनि तथा देवता भी सम्मिलित थे। महाराज दशरथ के पुत्र राम को जो देखता था उन्हें अपनी गोद में लेकर देखा और दूसरे की गोद में दर्शन करने दे दिया। दूसरे ने उन्हें देखा, फिर अपने पड़ोस में खड़े तीसरे को दर्शन करने दे दिया। जो भी उन्हें पाते थे, थोड़ी देर दर्शन किया, फिर वे उन्हें अपने पास नहीं रखते थे, दूसरों को दे दिया करते थे। यही हालत उस दिन, दिन भर रही।
सर्बस दान दीन्ह सब काहू। जेहिं पावा राखा नहिं ताहू ।।
भगवान राम सर्व के सर्वस्व है। इनको जो भी पाते गये, वे उन्हें अपने पास नहीं रख सके, अन्य को देते गये, यही सर्वस दान है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि भैय्या भरत! राम सर्व के सर्वस्व हैं। यदि सर्वस्व की रक्षा के लिए आधा का त्याग किया जाता है, तो बुद्धिमान जन इसे अनुचित नहीं मानते। अतः, तुम शत्रुघ्न के सहित जंगल में रहो तथा राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट जायँ, यही उचित दिखता है।
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई। फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ।।
सुनि सुबचन हरषे दोउ भ्राता । भे प्रमोद परिपूरन गाता ।।
गुरुदेव की इस वाणी को सुनकर भरत और शत्रुघ्न हर्षित हो गये, उनका हृदय आनन्द से भर गया।
कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हें। फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हें ।
कानन करउँ जनम भरि बासू । एहि तें अधिक न मोर सुपासू ।।
दोहा - अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान ।
जौं फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ।।256||
महात्मा भरत कहते हैं कि हे नाथ! भगवान राम से मेरे हृदय की बात छिपी नहीं है। वे तो अन्तर्यामी हैं और आप तो सर्वज्ञ हैं। मैं छलरहित विनयपूर्वक कहता हूँ कि मैं जीवन भर जंगल में रहना पसंद कर लूँगा। यदि आप जो कह रहे हैं, वह सत्य है तो, हे नाथ! आप अपनी इस बात को वापस न लीजिये। इसे प्रमाणित करके दिखाइये।
भरत बचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि भए बिदेहू ।।
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥
भरत के इन वचनों को सुनकर गुरु समेत सबके सब विदेह हो गये। महात्मा भरत के हृदय में राम और गुरु के प्रति जो प्रगाढ़ भक्ति है, वह निष्ठा ही अथाह सागर है और गुरुदेव की बुद्धि अबला स्त्री के समान है, जो इस पार खड़ी है वह उस पार जाना तो चाहती है, पर कोई साधन दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका भाव यह है कि गुरु वशिष्ठ सोचते हैं कि मैं यह क्या जानता था कि भरत इस तरह कमर कसकर तैयार ही हो जायेंगे, यही अगाध जलराशि (सागर) है। अब इस उलझन को मैं कैसे सुलझाऊँ। यही बुद्धि का अबलारूप है, क्योंकि वह तो वचन को प्रमाणित करने के लिए कह रहा है।
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज राम पहिं आए ।।
मुनि वशिष्ठ जी की अन्तरात्मा को भरत बड़े प्रिय लगे। अब इसी स्थिति में गुरुदेव सबको लेकर भगवान राम के पास पहुँचते हैं। यहीं पर पहली सभा महात्मा भरत की समाप्त होती है। अब यहाँ से आगे राम दरबार प्रारंभ होता है।
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु । बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ।।
भगवान राम ने गुरु के चरणों की वन्दना की और उन्हें सुन्दर आसन पर बैठाया। वशिष्ठ जी देश, काल और परिस्थिति का विचार कर कहते हैं कि हे राम ! तुम धर्म, नीति और ज्ञान के सर्वज्ञ हो।
दोहा- सबके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ कुभाउ ।
पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ।।257।।
गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम ! तुम 'मैं' नाम से सबके हृदय में स्थित हो और हर एक के हृदय के भाव और कुभाव को जानते हो, इसलिए इस राम दरबार में पुरजन, जननी और भरत इन सबका हित हो ऐसा निर्णय दीजिये।
भाई! यह राम दरबार है। इसमें न किसी की हार होती है, न किसी की जीत और न यहाँ के फैसले में किसी का अहित होता है। यह संसारी अदालत नहीं है, जहाँ एक की जीत और दूसरे की हार हो। एक सुखी होता हो, तो दूसरा दुःखी। ऐसा न्याय जीव दरबार में कहाँ हो सकेगा। जीव देशमें हार-जीत होती है, परन्तु राम देश में, नारायण देश में, अध्यात्म देश में न किसी की हार होती है, न किसी की जीत। बिना हार- जीत का फैसला वही कर सकता है, जो सारे चराचर का एक होगा, क्योंकि हार- जीत, राग-द्वेष, झगड़ा-लड़ाई दो में होती है, मगर भगवान आत्माराम सारे चराचर में एक हैं तो एक में ये सब कहाँ? जहाँ एक है, वहाँ सर्व का अभाव है।
जासु नाम सुमिरत इक बारा उतरहि नर भव सिन्धु अपारा ।
जानामु लेत भव सिंधु सुखाहीं करहु बिचारु सुजन मन माँही ।।
विचार करो कि 'मैं' कौन हूँ, भवसिन्धु क्या है? इस तरह विचार करना ही नाम लेना है, विचारों का जहाँ अन्त हो जायेगा। बस, भवसिन्धु सूख गया। रावण ने जीवन में केवल एक ही बार राम का नाम लिया था, "कहाँ राम रन हतौं पचारी" और फिर वह संसार में लौटकर नहीं आया। वह हमेशा राम को तपसी, स्त्रीबिरही, राजकुमार आदि ही कहा करता था। रावण बड़ा विद्वान और शिव का भक्त था।
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँति ।।
भगवान राम ने समुद्र के किनारे जब शिवलिंग की स्थापना की तब उनने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि भाई! इस समय रावण के समान महान विद्वान और पंडित विश्व में कोई नहीं है। अतः, तुम लंका में जाकर उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम कर हमारा संदेश कहो और उन्हें यहाँ लिवा लाओ, शिवजी का वह बड़ा भक्त है, हम शिव लिंग की स्थापना उन्हीं के द्वारा करायेंगे।
तद्नुसार, लक्ष्मण रामाज्ञा से वहाँ गये और नम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम कर राम का संदेश सुनाकर ले आये। भगवान राम ने उन्हें उनके चरण छूकर प्रणाम किया, जो कि क्षत्रिय यजमान का व्यवहार है। पश्चात् उनके द्वारा शिव लिंग की स्थापना हुई, अन्त में सब कार्य सम्पन्न हो चुकने पर भगवान राम ने उन्हें पुनः प्रणाम किया तब रावण राम को युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद देकर लंका लौट आये। लंका में आने पर उनके मंत्रिमंडल ने उन्हें बहुत प्रकार से उलाहना देते हुए कहा कि वहाँ जाकर यह आपने क्या किया, आपही से तो उनका युद्ध होना है और आपने ही उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया है। आपने यह अच्छा नहीं किया। इस पर रावण ने कहा भाई! तुम लोग इस बात को नहीं समझ सकते। अरे, पुरोहित रावण ने यजमान राम को आशीर्वाद दिया है, न कि राजा रावण ने। पुरोहित का कर्त्तव्य होता है कि वह अन्तःकरण से यजमान का हित चाहे। अतः, वहाँ मेरा वही कर्त्तव्य था और युद्ध तो राजाराम और राजा रावण से होना है। अतः, राजा रावण युद्ध करेगा। अस्तु, गुरु वशिष्ठ फिर सोचते हैं कि मैं स्वार्थवश कुछ का कुछ तो नहीं कह डाला, इस भावना से प्रेरित होकर वे फिर कहते हैं-
आरत कहहिं बिचारि न काऊ । सूझ जुआरिहि आपन दाऊ ।।
ऐसा कहकर अपने सिर का सारा भार उनने राम पर डाल दिया और समझने लगे कि चलो अब भार हलका हुआ, तब राम कहते हैं -
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ।।
इस तरह ऐसा कहकर भगवान राम ने रामावतार का सम्पूर्ण भार गुरु महाराज के सिर पर रख दिया। राम उस भार को एक मिनट के लिए भी तो अपने ऊपर रखते, वे कहते हैं कि हे गुरुदेव ! उपाय तो आपही के हाथों में है, मुझे आदेश दीजिये मेरे लिए क्या आज्ञा है।
सब कर हित रुख राउरि राखे । आयसु किएँ मुदित फुर भाषे ।।
हे गुरुदेव! तुम्हारा रुख देखकर काम करने में ही हम सबका कल्याण है।
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई । माथे मानि करौं सिख सोई ।।
हे नाथ! सबसे पहिले मुझे आज्ञा होनी चाहिए, बाद में फिर सबके लिए हो।
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा । भरत सनेहैं बिचारु न राखा ।।
गुरुदेव कहते हैं, भैय्याराम! तुम जो कहते हो सब सत्य है, परन्तु भरत की गुरु भक्ति ने मुझमें विचार की गुंजाइश नहीं रखी।
तेहि ते कहउँ बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भइ मति मोरी ।
मोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ।।
हे राम ! भरत की गुरु भक्ति ने मेरी बुद्धि को भोरी कर दिया है, इसलिए मैं बार- बार यही कहता हूँ कि भरत के विनय को आदर दिया जाये, फिर विचार किया जाये और ऐसा न्याय दिया जाये कि जिसको साधु, लोक और राजनीति सबका समर्थन मिले, जो श्रुति और सिद्धान्त का सार हो, निचोड़ हो।
दोहा - भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहोरि ।
करब साघुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ।।258।।
ऐसा कहकर भरत की पूरी-पूरी जिम्मेदारी गुरुदेव अपने सिर पर ले लेते हैं।
जीव की अदालत साढ़े तीन हाथ की होती है, क्योंकि वह साढे तीन हाथ की देह को ही अपना स्वरूप मानता है। तब जिसकी जितनी बड़ी मान्यता, उतनी ही बड़ी उसकी बुद्धि, पर यहाँ तो व्यापक, असीमित राम के दरबार का फैसला होना है, जो व्यापक फैसला होगा। अब इस भार को कोई भी एक मिनट के लिए भी अपने सिर पर नहीं रखना चाहता, क्योंकि यह भार सारे रामावतार का भार है। अतः, यह साधारण भार तो है नहीं। भरत गुरु के सिर पर, गुरु राम के सिर पर और राम फिर गुरुदेव के सिर पर इस तरह बोझ यहाँ से वहाँ फेंका जा रहा है।
गुर अनुरागु भरत पर देखी । राम हृदय आनंदु बिसेषी ।
भरतहिं धरम धुरंधर जानी। निज सेवक तन मानस बानी ।।
बोले गुर आयस अनुकूला । बचन मंजु मृदु मंगल मूला ।
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुअन भरत सम भाई ।।
जब गुरु ने भरत की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और इसको राम ने देखा कि गुरुदेव का अनुराग भरत पर है, तब भगवान राम ने भरत को मन, वचन और कर्म से अपना भक्त जाना और वे आनन्द विभोर हो कहने लगे कि हे गुरुदेव! मैं आपकी और पिता के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि भरत के समान भाग्यशाली विश्व में कोई नहीं है। जिस पर गुरु का प्रेम हो उससे बढ़कर संसार में कौन भाग्यशाली होगा?
जे गुरुपद अंबुज अनुरागी। ते लोकहुँ बेदहुँ बड़ भागी।
राउर जापर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू ।।
शिष्य में गुरु के प्रति नारायण भाव नहीं हो पाता, वह इसलिए कि वह गुरु को अपने ही समान क्रिया और व्यवहार करते देखता है। अतः, शिष्य के हृदय में उनके प्रति नरभाव ही होता है और गुरु में बिना नारायण भाव आये शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि कल्याण तो नारायण से ही होता है, नर से नहीं।
भगवान शंकराचार्य के आश्रम में कुछ विद्वान शिष्यमंडली वेदान्त पढ़ा करते थे। उनमें उनका एक अपढ़ शिष्य त्रोटक नाम का भी था, जो पढ़ा तो नहीं था, परन्तु उसके हृदय में प्रगाढ़ गुरु निष्ठा थी वह मन, वचन और कर्म तीनों से नित्य श्रद्धापूर्वक गुरु की हर तरह की सेवा किया करता था और नित्य इन विद्यार्थियों के समूह में बैठकर गुरुदेव के श्रीमुख से वेदान्त सुना करता था। एक दिन नियत समय पर भगवान शंकराचार्य के पास शिष्य मंडली वेदान्त पढने आ पहुँची। उस समय त्रोटक गुरुदेव के सब कपड़ों को धोने के लिए नदी में गया हुआ था। उन विद्यार्थियों के समूह में त्रोटक को न देखकर गुरुदेव उसकी प्रतीक्षा में शिष्यों को पाठ प्रारंभ न कर चुपचाप बैठे रहे। जब शिष्यों ने बड़ी देर तक उन्हें चुपचाप बैठे देखा तो उन्होंने पाठ प्रारंभ करने के लिए गुरुदेव से विनयपूर्वक आग्रह किया। इस पर भगवान शंकराचार्य ने कहा कि त्रोटक कहाँ है उसे भी आ जाने दो, फिर पाठ प्रारंभ हो। इस पर सब शिष्यों ने एक साथ कहा भगवन्! त्रोटक जो अपढ और मूर्ख है, उसकी बुद्धि वेदान्त ऐसे सूक्ष्म विषय को समझ सकने में समर्थ नहीं है। अतः, उसके कारण हमारा समय नष्ट न कीजिये और कृपाकर पाठ आरंभ कीजिये। शिष्यों के इस अनुरोध पर भगवान शंकराचार्य पाठ आरंभ करने वाले ही थे कि सामने से त्रोटक गुरुदेव के कपड़ों को धोकर नदी से आता हुआ दीख पड़ा। गुरुदेव ने कहा, वह देखो त्रोटक आ रहा है, उसे आ जाने दो। वह आया और धुले हुए सब कपड़ों को सूखने डालकर तुरन्त गुरुदेव के सम्मुख उपस्थित हो उनके श्रीचरणों की वन्दना कर, इन शिष्यों के एक ओर चुपचाप बैठ गया, तब गुरुदेव ने उसे अपने पास बुलाकर उससे कहा बेटा त्रोटक ! तुम्हारे ये सहपाठी तुम्हें अपढ़ और मूर्ख कहते हैं। अतः, तुम अपनी मूर्खता का कुछ परिचय तो इन्हें दे दो। ऐसा कहकर गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बस, फिर क्या था वह अपढ और मूर्ख त्रोटक वेदान्त के गूढ़ से गूढ तत्त्वों को वेदवाणी (संस्कृत) में ही धारा प्रवाह बोलने लगा और घण्टों बोलता रहा, जिसे देखकर अन्य शिष्य वर्ग के आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
यही त्रोटक आगे चलकर भगवान शंकराचार्य के चार प्रधान शिष्यों में से एक हुआ और इनका नाम त्रोटकाचार्य हुआ।
भैय्या! यह गुरु पर नारायण दृष्टि रखने के इतिहास का ज्वलन्त प्रमाण है। भगवान ब्रह्मा यदि किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसको वे सब कुछ दे देते हैं, परन्तु अपना ब्रह्मपद अर्थात् संसार की उत्पत्ति करने की शक्ति नहीं देते। भगवान विष्णु यदि किसी पर प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्त को सब कुछ दे डालते हैं, परन्तु अपना विष्णु पद अर्थात् संसार के पालन करने की शक्ति किसी को नहीं देते। ऐसे ही भगवान शंकर अपने भक्त को सब कुछ भले दे दें, परन्तु अपना शंकर पद याने सृष्टि के संहार करने की शक्ति किसी को भी नहीं देते। परन्तु, गुरु तो जिस पर वे प्रसन्न होते हैं, उसे अपना स्वरूप ही बना लेते हैं। एक दिया जलाया, फिर उस दिये से दूसरा दिया जलाया, उस दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से पाँचवाँ दिया जलाया गया। इस तरह परम्परा चल पड़ी। इसी तरह गुरु ने एक शिष्य को अपना स्वरूप बना लिया तो फिर वह दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवें को, आत्मज्ञान देते (अपना स्वरूप बनाते) चला जाता है। यह परम्परा चल पड़ती है।
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बड़ाई ।
भरतु कहहिं सोइ किएँ भलाई। अस कहि राम रहे अरगाई ।।
राम कहते हैं कि छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। छुद्र हृदय अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है और सन्त हृदय अपनी प्रशंसा सुनकर सिकुड़ जाता है।
जब राम ने सारा भार भरतजी पर डालकर कहा कि भाई भरत ! प्रसन्न मन से संकोच को त्यागकर साफ-साफ कहो कि तुम क्या चाहते हो। मैं वही करने को तैयार हूँ। तब इस प्रसंग पर अयोध्यावासियों का हृदय कमल तो खिल उठा, परन्तु देवतागण चिन्ता और शोक में डूब गये कि ऐसा न हो कि भरत प्रेमवश राम को अयोध्या न लौटा ले जायें, जिससे देवताओं का अहित हो जाये। देखो, अब विधाता क्या रंग लाते हैं। भरत कहते हैं कि हे नाथ! सबका स्वार्थ तो इसी में है कि भगवान अयोध्या चलें और इससे करोड़ गुना स्वार्थ तो इसमें है कि आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर स्वीकार किया जाय। भगवान, जैसा उचित समझें, वही हमारे कल्याण का कारण होगा।
भगवन्! मैं तिलक का सब साज सजा लाया हूँ, भगवान की जैसी इच्छा हो हमें वही करना है। हमें यही करना है, ऐसा हम नहीं कह सकते।
प्रथम बात तो यह है कि सरकार मुझे और शत्रुघ्न को वन भेज दें और आप सब अयोध्या चले। दूसरा, यह कि लक्ष्मण की जगह मैं आपकी सेवा में रहूँ और लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ अयोध्या लौट जायँ और तीसरी, विनय यह है कि हम तीनों भाई वन में जायें और माता सीता के साथ आप अयोध्या लौट चलें। ये तीन प्रस्ताव महात्मा भरत ने भगवान राम के समक्ष रखा अन्यथा सरकार की जैसी इच्छा, जो सब प्रकार से कल्याणप्रद ही होगा। इसलिए -
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिअ सोई ।।
भरत ऐसे कैसे कह सकते थे कि भगवान! आप अयोध्या ही चलें, क्योंकि क्या वे नहीं जानते थे कि रामावतार दुष्टों के विनाश के लिए, पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों की रक्षा के लिए ही हुआ है। इसलिए, ऐसा साफ-साफ नहीं कह सकते थे क्योंकि -
भरतहिं जानि राम परिछाहीं ।।
अन्त में वे कहते हैं कि हे नाथ!
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिअ सोई ॥
इस तरह भरत ने अपनी इच्छा भगवान राम के सन्मुख साफ-साफ रख दिया और फिर भगवान की इच्छा को ही प्रधान बताकर वहाँ से अलग हो गये, यही सभा चातुरी है कि सब कुछ कहकर अपने को वहाँ से अलग कर लिया, महात्मा भरत अन्त में फिर कहते हैं कि हे नाथ!
देवें दीन्ह सबु मोंहि अभारू । मोरें नीति न घरम बिचारू ।
कहउँ बचन सब स्वास्थ हेतू । रहत न आरत के चित चेतू ॥
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ।
अस मैं अवगुन उदधि अगाधू । स्वामि सनेहैं सराहत साधू ॥
अब कृपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि मन जाईं न पावा।
प्रभु पद शपथ कहउँ सति भाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ ॥
दोहा- प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब ।
सो सिर घरि-घरि करहिं सबु मिटिहिं अनट अवरेब ||269||
महात्मा भरत की इस वाणी को सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु-साधु की सराहना करते हुए उन्होंने पुष्पवृष्टि की, अयोध्या निवासी असमंजस में पड़ गये कि देखें अब श्रीराम क्या कहते हैं? तपस्वी तथा वनवासी लोग भगवान के वन में रहने की ही आशा से मन में परम आनन्दित हुए। अभी निर्णय कुछ नहीं हो पाया था, संकोची श्रीराम चुप ही थे कि इतने में ही -
जनक दूत तेहि अवसर आए। मुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए ।।
ठीक, उसी समय महाराज जनक के दूत सभा में आये, शिष्टाचार के बाद दूत राम का देश देखकर बड़े दुःखी हुए, जब उनसे जनकपुरी की कुशलता पूछी गयी तब वे कहने लगे, महाराज! वहाँ की कुशलता तो महाराज दशरथ के साथ ही चली गई।
महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार पाते ही महाराज जैसा कि उनका नाम विदेह है, विदेह हो गये। इसके बाद अयोध्या में गुप्तचर भेजकर उन्होंने वहाँ का समाचार जाना, तब उन्हें मालूम हुआ कि ब्राह्मण मंडल, प्रजा मंडल, मंत्रिमंडल, ऋषि मंडल और रानियों के मंडल राम के पास चित्रकूट चले गये हैं और अयोध्या सूनी पड़ी है, तब वे अपने मंत्रिमंडल और विद्वान मंडल से सलाह करके इस निर्णय में पहुँचे कि चित्रकूट ही चला जाये, तब वे तुरन्त वहाँ से दुघड़िया मुहूर्त साधकर चित्रकूट के लिए खाना हो गये। वे पास में आ ही चुके हैं। हम इसकी सूचना देने ही यहाँ आये हैं। महाराज जनक के आगमन को सुनकर अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हुए। वे सोचने लगे कि पिता और ससुर का दर्जा एक ही है, अब भगवान राम को अवश्य वे अयोध्या लौटने का संकेत करेंगे, जिससे हमारे दुःखों का अन्त हो जायगा।
महाराज जनक थोड़ी दूर स्फटिक शिला के पास आकर दण्डवत् करके पैदल चलने लगे और श्रीराम, भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर जनक की अगुवानी करने चले।
श्रीराम के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को भी रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है, क्योंकि मन तो श्रीराम और जानकी के पास है और बिना मन के शरीर के दुःख-सुख का अनुभव कौन करेगा? जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज समेत उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। दोनों दल जब पास में आये तो सब के सब प्रेम रस में डूब गये। फिर आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे।
जनक जी ने वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वन्दना की और श्रीरामचन्द्र जी ने जनकपुर से आये हुए ऋषियों, शतानन्द आदि को प्रणाम किया, फिर भाइयों सहित श्रीराम, राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले, मानसकार उस समय चित्र खींचते हैं, यहाँ से जनक दरबार प्रारंभ होता है।
दोहा- आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथ ।
सेन मनहुँ करुना सरित, लिएँ जाहिं रघुनाथु ।।275||
भगवान राम जहाँ निवास करते हैं, वह आश्रम सागर के समान है, वहाँ शांति रस का जल भरा हुआ है। वह पूर्ण भरा हुआ है, लबालब है, जो पावन है, अर्थात् पवित्र है, पाथ का अर्थ भी समुद्र ही होता है। महाराज जनक की सेना, सरित अर्थात् नदी के समान है, जहाँ करुणा का जल भरा हुआ है। इस करुणा नदी को श्रीराम भगीरथ के समान आगे-आगे चलते हुए अपने निवास आश्रम सागर में मिलाने ले जा रहे हैं। अब भाव समझो -
यह आश्रम चित्रकूट है, कूट का अर्थ द्रव्य होता है, जहाँ पर अनेक प्रकार के चित्र हों, उसे चित्रकूट कहते हैं, इस चित्त के अन्दर अनन्त चित्र हैं, इसलिये चित्त ही चित्रकूट है।
दोहा- रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु ।
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारू ||31||
इस चित्रकूट में श्रीराम आत्मा और शांति सीता बिहार करते हैं, जहाँ पर श्रीराम हों वहाँ पर अशांति का क्या काम?
अब अनुभव जगत् में आओ
सकल दृश्य निज उदर मेलि
इस सम्पूर्ण दृश्य जगत् को निज उदर अर्थात् निज स्वरूप भगवान आत्मा में विलीन करो-निश्चय करो कि- स एवाधस्तास उपरिष्टात्स-पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद सर्वमिति । अहमेवाघस्तादहमुपेरिष्ठादहं पश्चादहं दक्षिणातोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति । अर्थात् आत्मदेश आत्मै वाधस्तादात्मो परिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणगत आत्मोत्तरत आत्मैवेद सर्वमिति । वह ही नीचे है, वह ही ऊपर है, वह ही पश्चिम है, वह ही पूर्व है, वह ही दक्षिण है, वह ही उत्तर है, वह ही सब कुछ है।
'मैं' ही नीचे, 'मैं' ही ऊपर, 'मैं' ही पश्चिम, 'मैं' ही पूर्व, 'मैं' ही दक्षिण, 'मैं' ही उत्तर आत्मा ही सब कुछ है।
पूर्व समाधेरखिलं बिचिन्तयेदोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत् ।
तदेववाच्यं प्रणवो हि बाचको विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ॥
(अ.रा. उत्तर कां. 5 सर्ग 48)
इस स्थिति में अब जो प्रपंचाभाव का अनुभव हो रहा है, वही शांति रूपी जल से पूर्ण सागर है। इसका अनुभव चित्त में हो रहा है, यही चित्रकूट है, इसका जो अनुभव कर रहा है वह है राम, जो वहाँ निवास करते हैं। अब इस प्रपंचाभाव में शांति का अनुभव करो, क्योंकि अशांति तो प्रपंच में है, अब जब इसका अभाव हो गया तो शांति रस भरपूर हो गया यही श्रीराम का आश्रम है।
कोई भी विकल्प उठे, स्फुरणा उठे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कुछ भी हो, 'अहमेव' 'अहमेव' 'मैं' ही हैं, 'मैं' ही हूँ यही स्मरण करो, फिर तो इस शांतिरस से भरपूर, आश्रम का न आदि है, न मध्य है, न अन्त है, न इस पार है, न उस पार है।
अत्यन्त वैराग्य की फलानुभूति ही शांतिरस से पूर्ण सागर है यही भगवान राम का आश्रम है। भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि अत्यन्त वैराग्य का फल है निर्विकल्प समाधि और अत्यन्त वैराग्य उसे कहते हैं कि भगवान आत्मा के सिवा किसी के भी अस्तित्व को स्वीकार न करना इसका फल है निर्विकल्प समाधि और इस निर्विकल्प समाधि का फल है दृढ़बोध और इसका फल है नित्य सुख की प्राप्ति तथा समस्त बन्धनों से छुटकारा।
पूर्व समाधेरखिलं बिचिन्तये, दोंकार मात्रं सचराचरं जगत् ।
तदवे बाच्यं प्रणवो हि वाचको, विभाव्यते ज्ञानवशान्न बोधतः ।।
(राम गीता अध्यात्म रामा.)
समाधि के पहले यह अनुभव करें कि 'अहमेव' 'अहमेव' 'मैं' ही हैं, 'मैं' ही हूँ, यही अत्यन्त वैराग्य है, परम वैराग्य है।
कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ।।
अत्यन्त वैराग्यवान को ही निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है, अब यहाँ शांति ही शांति है। अरे! जब प्रपंच ही न रहा, तब शांति ही तो रह गयी। अत्यन्त वैराग्य का फल प्रपंच का नाश नहीं, प्रपंच का बाध है। डण्डे का नाश नहीं, डण्डा लकड़ी ही है, यह डण्डे का बाध है, इसी तरह आत्मबोध के बिना भी यह ऐसे ही दिखता है और बोध के बाद भी ऐसे ही दिखता है, मगर बोधवान की दृष्टि में प्रपंच का बाध है और अबोधवान की दृष्टिमें प्रपंच संसार है।
जब तक जगत् प्रपंच दिखाई दे रहा है, तब तक 'अहं' के साथ 'एव' लगा दो और जब प्रपंच न भासै तब एव कहोगे किसको? 'अहं' ही रह गया। मुक्ति रूपी अट्टालिका पर पहुँचने के लिए मुमुक्षु रूपी पक्षी के दो पंख होना चाहिए, एक वैराग्य और दूसरा ज्ञान। शरीर नहीं 'मैं' आत्मा हूँ, इसमें जीवभाव का अभाव हो गया और 'अहमेव' इसमें जगत् भाव का अभाव हो गया। अब आ जाओ प्रसंग पर-तो भैय्या! अत्यन्त वैराग्य की फलानुभूति की अनुभूति, शांतरस का अनुभव कौन कर रहा है? उत्तर है 'मैं' भगवान आत्मा कर रहा हूँ और अशान्त रस की अनुभूति ? उसे भी 'मैं' आत्मा ही करता हूँ। यहाँ न चित्त, न विषय, अहमेव। जो 'में' आत्मा निर्विकल्पता का अनुभव करता हूँ, वही 'मैं' आत्मा सविकल्पता का भी अनुभव करता हूँ, तथा इस निर्विकल्पता और सविकल्पता दोनों से परे 'मैं' आत्मा हूँ। यही राम का आश्रम है।
अब राम का अनुभव करो-
जहाँ हो, जैसे हो, जो हो, सोई रहो। न आँख मूंदो, न खोलो। अरे! जब आँख ही नहीं 'अहमेव' तब क्या मूंदोगे और खोलोगे। न देह है, न इन्द्रिय है और न संसार है। बस, यहाँ पर इनडायरेक्ट 'अहमेव' इसके बाद राम का दर्शन होता है। 'अहमेव' समाधि में निर्विकल्पता आ गई। अब, एव-फेव सब निकल गया, इनडायरेक्ट साधन पर निहित है और डायरेक्ट सन्त कृपा पर निर्भर है। प्रपंच दिखता है, तब अहमेव और जब अहं को देखा, तो प्रपंच कहाँ रहा? श्रीराम कहते हैं कि -
अत्यंत सूक्ष्मं परमार्थ तत्त्वं न स्थूल दृष्टया प्रतिपत्तु मर्हनि ।
समाधिनात्यन्त्यसु सूक्ष्मवृत्तया द्रष्टाव्यमायै रतिशुद्धिबुद्धिभिः ।।
समाधिनिष्ठ पुरुष को ही आत्मदर्शन हो सकता है और आत्मानुभूति में प्रपंचानुभूति की अभावानुभूति है। अर्थात्, मुझ आत्मदेश में प्रपंच नाम की चीज ही नहीं है। अब इस अवस्था में न तो निर्विकल्पानुभूति है और न सविकल्पानुभूति है। सिर्फ अनुभूति ही अनुभूति है। यही श्रीराम का दर्शन है। इस साधन में जो निर्विकल्पता आ गयी इस निरपेक्ष निर्विकल्पता का जो अनुभव कर रहा है, वही भगवान राम है। यहाँ जो शांति व्याप्त हो गयी यह सीता है। यह निर्विकल्पता है, यह सविकल्पता है, ऐसी विवेकनी जो बुद्धि है, वही लक्ष्मण है। चित्त जो स्थिर हो गया यही चित्रकूट है। यह जो कथा हो रही है, वही मंदाकिनी गंगा है। यह जो परम तत्त्व है, इसके प्रति जो निष्ठा है, वही चित्रकूट पर्वत है और उसी में सीताराम बिहार करते हैं। इस उत्तम सत्यानुभूति के बाद चलो अब थोड़ा चाल-चलन बनावें।
बोरति ग्यान बिराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे ।
सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तरुबर कर भंगा ।।
अब वह जनक की सेना रूपी करुणा नदी, आश्रम रुपी सागर में मिलने चली तो यह करुणा नदी ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों कगारों को डूबाते चली जा रही है। मिथिलापुरवासियों के शोक भरे वचन कि अयोध्यापति का निधन हो गया है, अयोध्या सूनी है, श्रीराम वन आ गये हैं, राजसिंहासन खाली पड़ा हुआ है। इस स्थिति में कोई शत्रुराजा वहाँ चढ़ाई न करदे। हा विधाता ! क्या होने वाला है अथवा कैसा होगा, यही नदी और नाले इस करुणा नदी में आ-आकर मिल रहे हैं। उनके मुख से चिन्ता और शोक में डूबे हुए जो लम्बी-लम्बी सांसे निकल रही हैं, यही उस बढ़ी हुई नदी की तरंगे हैं, जो किनारे के धीरज रूपी वृक्षों को उखाड़-उखाड़कर फेंकने वाली हैं।
विषम विषाद तोरावति धारा। भय भ्रम भर्वैर अबर्त अपारा ।
केवट बुध विद्या बड़ि नावा। सकहिं न खेइ ऐक नहिं आवा ।।
भयानक शोक ही उस नदी की तेज धार है, उसके मन में जो तरह-तरह के तर्क और भय हो रहा है, यही उस नदी के असंख्य भँवर हैं। बड़े-बड़े विद्वान, ऋषि, मुनि इस भयंकर बढ़ी हुई नदी से पार करने वाले केवट के समान हैं। उनकी बुद्धि ही नाव है। इस नाव पर चढ़कर पार हो जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है।
बनचर कोल किरात बिचारे । थके बिलोकि पथिक हियँ हारे ।
आश्रम उदधि मिली जब जाई। मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई ।।
वन में विचरने वाले विचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार मानकर थक गये हैं, यह करुणा नदी जब आश्रम सागर में जाकर मिली तो मानों वह समुद्र अकुला उठा।
सोक बिकल दोउ राज समाजा। रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा ।
भूप रूप गुन सील सराहीं । रोवहिं सोक सिन्धु अवगाहीं ।।
दोनों राज समाज शोक में व्याकुल हैं। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और ति लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे आज हैं और शोक सागर में डूब रहे हैं।
सोरठा -
किए अमित उपदेस जहँ तहँ लोगन्ह मुनिबरन्ह ।
धीरजु घरिअ नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ।।
(सो. 276)
मुनियों ने लोगों को अनेक प्रकार से उपदेश दिये और वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी से कहा कि हे राजन! आप धैर्य धारण कीजिये।
जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल बिकासा।
तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई ।।
महाराज जनक का ज्ञान सूर्यवत् प्रचण्ड प्रकाशवान है। उनके वचनरूपी किरणों के द्वारा बड़े-बड़े ऋषि, मुनियों का भी हृदय कमल खिल उठता है। ऐसा जिनका हो ज्ञान प्रकाश है, ऐसे विदेहराज आत्मनिष्ठ राजा जनक विदेहमुक्त को क्या मोह ममता हो सकती है, जो रो रहे हैं? नहीं! अरे! यह तो सियाराम के विशुद्ध प्रेम की महिमा है। मनुष्य को ज्ञान सिखाना पड़ता है, परन्तु पशु-पक्षी को ज्ञान नहीं दिया जाता फिर भी वे ज्ञानी हो जाते हैं, कारण यह है कि जहाँ पर एक भी ब्रह्मनिष्ठ रह जाता है, वहाँ के वायुमंडल में सन्त भावना के परमाणु उसके आसपास नित्य व्याप्त रहते हैं। गौतम बुद्ध ने जिस स्थल पर अहिंसा का तप किया था, वहाँ के रहने वाले सभी हिंसक पशु संत भावना से परिपूर्ण, राग-द्वेष से रहित हो, वन में विचरते रहते थे। कागभुसुण्डी के आश्रम में योजन भर तक काम, क्रोध, लोभ, मोह का नामोनिशान तक नहीं था। प्राचीन और अर्वाचीन सन्त महात्माओं के आश्रम में रहने वाले कीट-पतंग तक आपस में राग-द्वेष को भूलकर सब एक साथ एक रूप में रहते हैं। इसी प्रकार महाराज जनक इतने विदेहमुक्त थे कि इनके सम्पर्क में रहने वाले कीट, पतंग, पशु, पक्षी सभी ज्ञानी थे। उनके यहाँ तोता, मैना भी ज्ञानी थे, जिनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए महात्मा व्यास के पुत्र महाविरक्त शुकदेव को भी जाना पड़ा था। इसी तरह बड़े- बड़े योगी, ज्ञानी उनके पास आत्म साक्षात्कार के लिए जाया करते थे, ऐसे ज्ञानी जनक की आँखों से राम और सीता को मुनिवेश में देखकर अश्रुपात होने लगे, तो यह मोह जनित कर्म नहीं है, वे सीता-राम के विशुद्ध प्रेम में रो रहे हैं, न कि मोह ममता में। यदि ज्ञानी को भी मोह हो गया तो -
तरति शोकमात्मवित् विद्वान शोक मोहोजहाति ।।
यह श्रुति किसकी शरण में जायेगी? राम के वनवास को सुनकर जब भरत अत्यन्त व्याकुल और दुःखी हुए, तब कौशल्या उन्हें धीरज देते हुए कहती है कि-
बिधु बिष चुवै हिमु आगी। होइ बारिचर बारि बिरागी ।।
भएँ ग्यानु बरु मिटै न मोहू। तुम्ह रामहिं प्रतिकूल न होहू।
इससे यही सिद्ध होता है कि ज्ञानवान को स्वप्न में भी मोहनहीं हो सकता।
संसार, स्त्री, पुत्र, धन, परिवार के लिए रोता है, परन्तु भगवान राम के लिए उनके प्रेम में रोना ही, सचा रोना है क्योंकि -
रामहिं केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जाननहारा ।।
परन्तु, प्रेम तो बाहर की चीज नहीं है, यह तो भीतर की चीज है, जैसे कछुआ अपने अण्डे का भीतर से मन ही मन चिन्तन करते रहता है, उसी प्रकार जब चिन्तन होने लगे, तब समझना कि यह राम प्रेम है।
जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु ।।
जिस स्नेह में विधि निषेध हो वह बनावटी स्नेह है और जिसमें विधि निषेध का अभाव हो, वह सहज रनेह है, जैसे पुत्र के प्रति पिता का, पति के प्रति पत्नी का सहज स्नेह होता है। ये आपस में समयानुसार लड़ते झगड़ते हैं, फिर भी भीतर स्नेह ज्यों का त्यों बना रहता है।
शमां के रूबरू आकर, शमां में जलते परवाने ।
मुहव्वत अंदरूनी में, शमां जाने या परवाने ॥
भैय्या! सहज स्नेह का यह एक नमूना है। विषई साधक सिद्ध सयाने । त्रिबिध जीव जग बेद बखाने । राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभाँ बड़ आदर तासू ।।
देखो तीन प्रकार के जीव होते हैं, विषयी अर्थात् कर्मकाण्डी, साधक अर्थात् उपासक और सिद्ध सयाने अर्थात् ज्ञानी। ज्ञानी भी जीव ही है, क्योंकि वह भी अपने मैं को देह, जीव न मानकर ब्रह्म मान रहा है, तो कुछ न कुछ मानते रहना यह जीव भाव ही है। इसलिए मानसकार ने तीनों को जीव ही कहा, इन तीनों में से किसी का भी मन राम स्नेहमें डूब गया तो सन्त समाज में उसका बड़ा आदर होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं, तब यद्यपि वह मूर्ति पत्थर ही है, परन्तु उसमें हम भगवान की भावना करते हैं और जितनी देर तक हम उस मूर्ति भगवान के सामने
सोह न राम पेम बिनु ग्यानु। करनधार बिनु जिमि जलजानू ॥
खड़े रहते हैं तब तक हमारे चित्त में इस प्रकार निर्विकल्पता आ जाती है कि उतनी देर तक हम सारे द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं। एक स्थान में ही थोड़ी देर तक भगवान की भावना होने का तो यह फल है तब जो नित्य सारे चराचर को अपना आप भगवान आत्मा जानता है, जिसकी दृष्टि में सर्व वासुदेव है, आप सहित सारा विश्व भगवान राम है और चौबीस घंटे जिसका मन उसी में डूबा रहता है तो भला उसकी क्या दशा होती होगी, इस प्रकार भगवान राम में जिसका मन डूबा रहे, गल जाये, यही राम प्रेम है। जलयान जो नाव है, वह बिना केंवट के भला कैसे पार लगेगी, इसी प्रकार ज्ञान नाव है और राम प्रेम जो है, वह इस नाव का खेने वाला कर्णधार केंवट है।
'अहं ब्रह्मास्मि' यह है ज्ञान। प्रश्न होता है कि यह मानना है या सिद्धान्त है? उत्तर है- यह मानना है, भावना है।
'मैं' ब्रह्म हूँ, इसको अनुसंधान कहते हैं, यह आखिरी मंजिल नहीं है। मैं आत्मा यदि न होऊँ, तो ब्रह्म भाव किस पर आरोपित होगा, यह किस पर आधारित होगा? 'अहं ब्रह्मास्मि' यह जो भावनात्मक ज्ञान, वृत्तिजन्य ज्ञान, क्षणिक ज्ञान अनित्य ज्ञान, किसी महापुरुष की शरण में जाकर श्रवण, निदिध्यासन द्वारा वृत्तिम जो पैदा हुआ ज्ञान है, उसमें अभी पूर्ण रूप से बोध नहीं हुआ तो नाव डगमगाती ही रहेगी। अरे, ज्ञानी तो जीव ही है। गरीब को ही अमीर बनने की इच्छा होती है। ब्रह्म को क्या जरूरत है कि 'मैं' ब्रह्म हूँ कहे। तब यह तो आत्मतत्त्व है, यह है कर्णधार जब इसका बोध न हुआ, तब जैसे आज ब्रह्म माना है, वैसे ही कल फिर जीव मान लेगा, क्योंकि नित्य अज्ञानी जीववादियों के ही संसर्ग में रहना है, तो संग दोष का प्रभाव होना ही है। परन्तु 'मैं' हूँ यह भी क्या अनुसंधान है? बस, यही जलयान है। इस नाव पर चढ़कर ही पार हुआ जा सकता है। ब्रह्म भाव में शोक, मोह, दुःख-सुब चिंता सभी है। 'यावनाहं "मैं' जैसा हूँ, यह रह जाय, यही राम प्रेम है। आत्मतत्त्व के बोध का यही स्वरूप है कि आज के पहिले 'मैं' क्या था, अभी क्या हूँ, आगे क्या रहूँगा, इसकी स्मृति का अत्यन्ताभाव हो जाय यही पूर्ण बोध है। जिस प्रकार नदिय को समुद्र में मिलने के बाद यह स्मृति नहीं रहती कि आज के पहिले मैं अमुक थी। यहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों नहीं रहते, इसी पद को वेदों के शब्दों में 'भवहरणिभनि कहा है।
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी ।
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि पतत हम देखत हरी ।।
यह वेद स्तुति है। इसका भाव यह है कि माने हुए ज्ञान में उन्मत होकर तुम्हा 'भवहरणि भक्ति' याने संसार से तारने वाली भक्ति का जो आदर नहीं करता भगवन्! उसे हम पतन होते देखते हैं। राम प्रेम ही भवहरणि भक्ति है, राम प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही राम है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, इस का स्वाद सबके अन्तःकरण में प्रदर्शित नहीं होता यह तो बिरले ही गुरु नैहिक भाग्यशाली को ही प्रतीत होता है। 'मैं' पद की स्थिति (जो अमानी पद है) में प्रमाद का अत्यन्ताभाव है।
भगवान ने ज्ञानी को प्रौढ तनय कहा है और अमानी भक्त को जो अपने 'मैं' को कुछ नहीं मानता, 'मैं' का 'मैं' ही जानता है, उनके अन्तःकरण में जगत् प्रपंच 'मैं' आत्मा ही अनुभव होता है, ऐसा अमानी भक्त, मेरा छोटा शिशु है, जिसकी रखवाली मुझे नित्य माता के समान करनी पड़ती है।
रामहि केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जानन हारा ।।
"मान लेहु जो मानन हारा" नहीं कहा, "जानलेहु जो जानन हारा" कहा गया। बस, यहीं पर जनक सभा का अन्त होता है। अब रानियों की सभा प्रारंभ होती है-
महाराज जनक की महारानी सुनयना ने महारानी कौशल्या के पास अपनी दासी भेजकर उनसे मिलने के लिए आज्ञा मांगी और उनके द्वारा जब आज्ञा मिल गयी, तब वे अन्य रानियों को लेकर राजा दशरथ की रानियों के समाज में जाकर मिलीं। यहाँ महाराज दशरथ की तीन रानियों का प्रसंग है, जो प्रमुख थीं, यद्यपि उनकी और बहुत-सी रानियाँ थीं। इसी प्रकार जनक की भी बहुत-सी रानियाँ थीं। दोनों समाज की सब रानियों ने मिलकर शोकसभा मनायी, दोनों ओर की रानियों के शील और प्रेम को देखकर तथा सुनकर कठोर वज भी पिघल जाते हैं। सबके शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आँसू हैं। सबके सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेद रही हैं और शोक सागर में डूबी हुई हैं, सभी श्री सीता और राम के प्रेम की मूर्ति ही हैं, वे इस समय ऐसा जान पड़ती हैं मानो स्वयं करुणा ही अनेक रूप धारण करके दुःख से बिसूर रही हो, इस प्रसंग पर सीता जी की माता सुनयना कहती हैं-
सीय मातु कह बिधि बुधि बाँकी। जो पय फेनु फोर पबि टाँकी ।।
पवि कहते हैं, हीरा को। असली हीरा वही है, जो हथौड़ा के सैकड़ों चोट लगने पर भी न फूटे, परन्तु उसी हीरे पर यदि दूध के फेन रखकर जरा-सा मार दो तो वह तुरन्त दो टुकड़ा हो जाता है। माता सुनयना की सभा चातुरी देखो वे कहती हैं कि हाय रे विधाता! श्रीराम राज्याभिषेक रूपी वज्र को फोड़ सकने की विश्व में किसी की ताकत नहीं थी, परन्तु इस राम राज्याभिषेक रूपी वज में कैकई के दो वरदान रूपी दूध के फेन को रखकर मन्थरा रूपी हथौडे से तूने फोड़ दिया, तेरी बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। वह इस प्रकार कह रही है कि इसका भाव समझने वाला ही समझे।
दोहा - सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल, सब करतूति कराल ।
जहँ तहँ काक, उलूक, बक, मानस सकृत मराल !!281।।
सुनयना कहती हैं कि संसार में सुनने में तो आता है अमृत, परन्तु आज तक किसी ने अमृत देखा नहीं। सबको विष ही दीख पड़ता है। सुनते हैं कि मानसरोवर में हंस है, परन्तु आज तक उन्हें किसी ने देखा नहीं, केवल कौवे, उल्लू और बगुले ही दीख पड़ते हैं। कभी-कभी मैं अपने महाराज विदेहराज से पूछती थी कि महाराज! अयोध्या नरेश कैकई पर इतना प्रेम क्यों करते हैं? तो इसके उत्तर में वे कहते थे, कि कैकई के कण्ठ में अमृत है, वह अत्यन्त मधुर भाषिणी है, इसीलिए महाराज उस पर अधिक प्रेम करते हैं, तब जिस कण्ठ में अमृत का वास हो वहीं से राम बनवास रूपी विष निकला, मधुर भाषिणी का क्या यही अर्थ है कि वहाँ से बनवास रूपी कठोर शब्द निकले। कैकई काक वृत्ति वाली है, कौवा किसी पर विश्वास नहीं करता। अयोध्या नरेश ने उन्हें कई तरह से वचन दिया, शपथ खाया, 'नाहिंन राम राजकर भूखे आदि। परन्तु, इस कौवे रूपी कैकई को विश्वास नहीं हुआ। सूर्यवंश का सूर्य अयोध्या नरेश का निधन हो गया। अयोध्या में सर्वत्र शोक, अन्धकार छाया हुआ है, उसमे यह कैकई उल्लू की तरह जीवित है। यह बगुला है, जो अयोध्यापति के प्राण रूपी मछली को निगल गयी। इस तरह सुनयना को शोकवश आपे से बाहर उत्तेजित और विक्षुब्ध हुए देखकर सुमित्रा, उसे धैर्य बँधाने और शांत करने के लिए, शोक के साथ कहती है-
सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा । बिधि गति बड़ि बिपरीत बिचित्रा ।
जो सृजि पालइ हरइ बहोरी। बाल केलि सम बिधि मति भोरी ॥
हे बहिन! विधाता की बुद्धि बच्चों की बुद्धि जैसी है, जो स्वयं बनाता है, फिर उसका पालन करता है और फिर स्वयं नष्ट कर देता है।
इसके बाद माता कौशल्या कहती है कि -
कौसल्या कह दोसु न काहु । करम बिबस दुख सुख छति लाहू।
कठिन करम गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥
ईस रजाइ सीस सबही के । उतपति थिति लय विषहु अमीके ।
देबि मोह बस सोचिअ बादी । बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥
इसलिए हे देवि! इसमें किसी का दोष नहीं है, दुःख-सुख, हानि-लाभ, सब कर्म के अधीन हैं, कर्मों की गति बडी कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। इसलिए, मोहवश सोच करना व्यर्थ है. क्योंकि विधाता का यह प्रपंच, अचल और अनादि है।
विधाता के इस प्रपंच को माता कौशल्या ने अचल और अनादि कहा, विषय समझो कि यह प्रपंच अचल और अनादि किस तरह है -
अचल का अर्थ है जो चलायमान न हो और अनादि का अर्थ है जिसका आदि न हो, अर्थात् यह कब से है इसके शुरुआत का पता न हो। यदि इसे कोई पैदा किया होता तब अनादि न कहा जाता। अनादि कहने से इसका पैदा होना सिद्ध नहीं होता, परन्तु यह प्रपंच आज कुछ है और कल कुछ और है। आज उत्पत्ति है तो कल पालन है, फिर संहार है तो यह अचल कैसा हुआ?
तो इसका उत्तर यह है कि इसका जो चलपना है वह तो अचल है, यह जो परिवर्तनपना है वह तो अचल है, इसको तो कोई टाल नहीं सकता। इसलिए यह प्रपंच अचल है और चलपना परिवर्तनपना, कब से है, इसके शुरुआत का भी कुछ पता नहीं है। इसलिए अनादि भी है, यह तो चलपने का प्रवाह है, वह भी अचल है। यह चल इसलिए अचल है कि यह अनादि है, अर्थात् चल कब से इसका कोई जन्म सम्वत् नहीं, जहाँ संसार प्रपंच को अनादि कहा कि इसका अचलपना स्वयं सिद्ध हो जाता है।
स्वतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते ।
सदसत्सदसद्वापि न किंचिद्वस्तु जायते ॥
(गौ. कारि.अ.शा.प्र.-22)
अर्थात् न सत की उत्पत्ति होती है, न असत ही उत्पन्न होता है और न सत्- असत दोनों की उत्पत्ति होती है। यदि सत् पदार्थ की उत्पत्ति मानोगे तो उत्पन्न हुआ पदार्थ नाशवान होता है, तब इसे सत् कैसे कहेंगे? क्योंकि, सत् वस्तु तो त्रिकाला बाघ होती है और यदि असत् की उत्पत्ति मानोगे तो असत् बन्ध्यापुत्र वत् होता है। याने जो है ही नहीं वह पैदा क्या होगा? तात्पर्य, यह है कि किसी प्रकार से भी, किसी भी देश, काल, वस्तु का उत्पन्न होना सिद्ध नहीं होता। यदि, जगत् प्रपंच को ईश्वर में पैदा किया मानों तो वह ईश्वर जिसने इसे पैदा किया जन्मा है या अजन्मा ? माही। क्योंकि, ईश्वर तो अविनाशी है, जन्म-मरण से रहित है। यदि कहो अजन्मा है तो कहा जन्मा है तो यह मेराहा, अश्या कि जो जन्म लेता है वह मरता है तो वह ईश्वर सूतो अजन्मा से क्या पैदा होगा? जो स्वयं पैदा नहीं हुआ उसे दूसरे को पैदा करने की क्या तमीज? इसलिए, प्रपंच पैदा हुआ ही नहीं। यही उत्तम सत्य है, इसी को वेदान्त में 'अजात्वाद' कहते हैं।
प्रपंच देश से प्रपंच चल है और अचल देश से प्रपंच चल, अचल है तो चल है, वह अचल ही तो है और अचल भगवान आत्मा ही तो है। इस स्थिति में प्रपंच का विकल्प ही कहाँ ? अचल देश से देखो तो प्रपंच की गुंजाइश ही नहीं। एक बार भगवान राम ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा भगवन! आप तो बहुत बड़ी आयु वाले हैं, यह प्रपंच कब से बना, इसे आप जानते हैं, दयाकर बताइये कि यह संसार कब बना?
तब गुरुदेव कहने लगे राम! मुझे अपनी उम्र का ठीक-ठीक पता तो नहीं है, परन्तु मैंने अपनी आँखों से बहत्तर त्रेतायुग देखा है, पर मैं इसे ऐसा ही देख रहा हूँ। मुझसे ज्यादा सयाना भुशुण्डी है, एक बार उनसे भी मैंने यही प्रश्न पूछा था, तब उनने कहा कि यह प्रपंच कब से है, यह तो मैं नहीं जानता। मैंने आठ वशिष्ठ देखा है और ग्यारह ब्रह्मा मेरे सामने मरे हैं। चारों युग जब एक हजार बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, ब्रह्मा अपने दिन से सौ वर्ष की आयु में मर जाता है। सत्रह बार मैंने रामावतार देखा है, कभी नारी-नारी की सृष्टि देखा, तो कभी नर-नर की। कभी राख ही राख देखा है, तो कभी जल ही जल देखा, परन्तु मुझे भी यह नहीं मालूम कि यह कब से बना, भुशुण्डी ने कहा, कि हमारे गुरुदेव लोमश हैं, ब्रह्मा का सौ वर्ष हमारे गुरुदेव का एक दिन है, उनके एक दिन में रोज एक ब्रह्मा मरता है, इस तरह उन्हें रोज सूतक लग जाता है तो वे रोज कहाँ तक बाल बनवाते रहें, वे अपनी जटा से रोज एक बाल उखाड़कर फेंक देते हैं। उन्हें भी यह नहीं मालूम कि यह कब से बना। इस तरह यह प्रपंच अनादि और अचल है।
प्रश्न होता है कि जब प्रपंच अचल और अनादि है और इसका कर्त्ता कोई नहीं है, तब फिर वह क्या है?
उत्तर है-वह इस विकल्प के अभाव का भाव है। प्रपंच का अचलत्व, प्रपंच नहीं है अचल है, प्रपंच का अनादित्व प्रपंच नहीं है अनादि है। इस तरह यह प्रपंच, प्रपंच नहीं आत्म सत्ता है, अस्तित्व ? ज्यों ही भगवान आत्मा अस्तित्व को संसार माना कि इसके लिए चार विकल्प आकर सामने खड़े हो गये। देश, काल, वस्तु और कत्र्ता। कहाँ बना, कब बना, किससे बना और किसने बनाया। इन विकल्पों के होते ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश सामने आ गये। अस्तित्व को खिसका लो तो संसार ही नहीं और जब संसार ही नहीं तो फिर इसके सृष्टा, भर्ता और हर्ता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं। इस तरह न कोई संसार, न कोई इसके उत्पत्ति, पालन और संहारकर्ता। रह गया 'मैं' विशुद्ध तत्त्व भगवान आत्मा।
पुराणों में अलंकारिक कथाएं हैं, परन्तु आजकल क्या होता है कि जिस प्रकार छोटे-छोटे बच्चों को झूठ बोलने के परिणाम बताने के लिए कोई मनगढन्त कहानी सुनायी जाती है, मगर बच्चा कहानी को ही ग्रहण कर लेता है और अधिक झूठ बोलना सीख लेता है। उस कहानी के तात्पर्य अथवा सारांश को छोड़ देता है, जिसके लिए उसे कहानी बतायी गयी थी। इसी प्रकार संसारी जीव पुराणों, शास्त्रों में बताये गये कथा भाग को ही पकड़ लेते हैं और सारांश अथवा तात्पर्य को छोड़ देते हैं। इस तरह उनसे सत्य वस्तु तो छूट जाती है और मनगढन्त, असत्य, कल्पना ही उनके हाथ लगती है। इस पर एक दृष्टान्त सुनो-
किसी जंगल में एक कैथ के पेड़ के नीचे एक खरगोश का बिल था, जिसमें वह रहा करता था। एक दिन बिल में पड़े-पड़े उसके मन में कल्पना उठी कि यदि धरती उलट गयी तो कैसा होगा? इस जंगल का क्या होगा? यहाँ के पेड़, पौधे तथा यहाँ रहने वाले पशु, पक्षी कैसे करेंगे? बस, इस असत्य कल्पना ने उसे बेचैन कर दिया। वह रात भर यही सोचता रहा और परिणाम से घबराता रहा। निदान, सुबह होते ही वह जंगल में भोजन की तलाश में चल पड़ा। वह शाम को जब अपने बिल में आता तब नित्य उसके मस्तिष्क में यह विकल्प उसी ताजगी से उठता कि यदि धरती उलट गयी तो कैसा होगा? और नित्य उसे इसी चिंता में रात बितानी पड़ती। एक दिन वह इसी कल्पना से चिंतित अपने बिल में पड़ा था कि जोर की हवा चलने से कैथ का बड़ा फल उसके बिल के दरवाजे पर धमाक से गिरा। बस, फिर क्या था, वह समझ गया कि अब धरती उलट रही है और झटपटाकर, उठकर जंगल में एक ओर यह कहते हुए जोर से भागा कि "भागो रे, धरती उलट रही है, भागो रे, धरती उलट रही है।" जंगल के जो भी जानवर खरगोश की इस घबराहट भरी आवाज को सुनते गये, सब उसी ओर जिधर कि खरगोश भाग रहा था यही कहते हुए भागने लगे कि- "भागो रे धरती उलट रही है।" निदान, जंगल में जंगली जानवरों के भाग-दौड़ की धूम मच गयी। सियारों, भेड़ियों, हिरणों, हाथियों, चितों आदि सम्पूर्ण जंगली जानवर दल के दल जोर से यही कहते हुए भागने लगे। इनकी भाग-दौड़ में जंगल का राजा सिंह जो अपनी गुफा में सुख की नींद सो रहा था, जाग उठा।
वह अपनी गुफा से बाहर आया और उसने जंगल में इन जानवरों को घबराये हुए एक ओर जोरों से भागते हुए देखा। तब उस सिंह ने ललकार कर उन सबको तुरन्त वहीं रुक जाने को कहा। उसकी एक ही ललकार में सबके सब जो जहाँ थे, वहीं खड़े हो गये। तब उस सिंह ने सामने खड़े हुए जानवरों से पूछा, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तब सामने खड़े हुए जानवरों ने उन्हें उत्तर दिया- हुजूर! धरती उलट रही है। इस पर सिंह ने पूछा कि धरती किधर से उलट रही है। तब उन जानवरों ने कहा- सरकार! यह तो हम नहीं जानते। आगे भागने वाले बतायेंगे जिनसे सुनकर हम भाग रहे हैं। तब सिंह ने उनके आगे वाले जानवरों से पूछा-उत्तर दिया महाराज! यह हम भी नहीं जानते कि किधर से धरती उलट रही है। यह तो हमने अपने आगे भागने वाले जानवरों से सुना है, आगे वाले ही जानेंगे। निदान, इस तरह घण्टों पूछते-पूछते अंत में खरगोश की पारी आयी। जब सिंह ने उससे भी वही प्रश्न किया तब खरगोश हाथ जोड़कर कहने लगा कि हुजूर! धरती मेरे बिल के पास उलट रही है। ऐसा कह उसने सिंह को ले जाकर अपने बिल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। तब उसने देखा कि बिल के दरवाजे पर कैथ का एक बड़ा फल झाड़ से गिरा था और उसी की आवाज से इस खरगोश ने अपने द्वारा ही किये गये असत्य कल्पना से भयभीत होकर यह आंदोलन शुरू किया था। इसी प्रकार आजकल के कथावाचक, श्रोता लोग खरगोश के समान हैं। कथावाचक कहते हैं कि ! भवसागर से पार होओ, संसार-सागर से तरो। उनका यह आंदोलन चल पड़ा है। बस, सब श्रोता इसे सुनकर इसी की रट लगाते हुए घबराहट और चिंता से ग्रसित हैं। जब कोई सन्त, महात्मा जन सिंह के समान सामने आकर उनसे पूछते हैं कि कहाँ है भवसागर जिसे तरने कह रहे हो? कहाँ है संसार-सागर जिसे पार होना है? तब वे उन जानवरों के समान कुछ नहीं बता सकते, बताएँ कहाँ से भवसागर हो तब तो उसे दिखाएँ, संसार हो तब तो वह दिखाया जाए, यही असत्य कल्पना से भय है। इसीलिए कौशल्या ने विधि प्रपंच को अचल और अनादि कहा। अस्तित्व भगवान आत्मा भास को ही संसार मान लिया। भगवान पर ही संसार की असत्य कल्पना कर ली गयी और इसी अपने द्वारा की गयी असत्य कल्पना में ही सब घबराहट और चिंता है।
जब भगवान आत्मा 'मैं' का बोध हो जाता है, तब सर्व दुःखों से क्षण मात्र में छुटकारा मिल जाता है तथा सर्वदा के लिए परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न होता है कि श्रुति भी जगत् की उत्पत्ति बताती है भाई! जगत् की उत्पत्ति तो बताती है, फिर अपवाद भी तो कर देती है, किस प्रकार देखो -
अध्यारोपापवादाभ्यां ……………………………… अखिलं प्रपंच्यते ।।
जो परमात्मा ब्रह्म, सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मा को समाधि अवस्था में वेद सुनाया, जिनकी कृपा से वेद प्रकट हुए उनकी शरण में मैं हूँ। इससे मालूम होता है कि संसार पैदा हुआ है, लेकिन आगे चलकर श्रुति यह भी तो कहती है कि -
एकमेमाद्वितीयो ……………………………….. नेहनानास्ति किंचन ।।
एक ही चेतन परमात्मा है इसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। श्रुति के वाक्य में इतना विरोधाभास। तो कहते हैं, यहाँ विरोधाभास नहीं है पूर्वा पर विरोध नहीं है, वह अध्यारोप है और यह अपवाद है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कन्ध के एकसठवें अध्याय का पहला श्लोक में कहते हैं -
एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबलाः ।
अजीजनन्ननवमान्पितुः सर्वात्मसम्पदा ।।
(श्रीमद् भागवत 10-61-1)
श्रीकृष्ण महाराज की सोलह हजार एक सौ आठ रानियों से एक-एक से दस-दस पुत्र हुए। फिर, उसी के नीचे के चौथे श्लोक में श्री शुकदेव जी कहते हैं -
स्मायावलोकलवदर्शितभावहारि भ्रूमण्डल प्रहित सौरतमन्त्रशौण्डेः ।.
पत्नयस्तु षोडशसहस्त्रमनगङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न शेकुः ।।
(श्रीमद् भागवत 10-61-4)
तो क्या पुत्र आसमान से आये? कहाँ से आये? सोलह हजार एक सौ आठ रानियों के मध्य में रहते हुए भी कामदेव भगवान श्रीकृष्ण के काम प्रदीप करने में समर्थ नहीं हुए। बिल्कुल उलट गया। यह क्या है? तो यह अध्यारोप और अपवाद है। बिना आत्मबोध हुए यह बात शीघ्र समझ में नहीं आती। इसमें हर एक रानियों के दस-दस पुत्र हुए यह अध्यारोप है और भगवान श्रीकृष्ण आप्तकाम हैं। उन पर काम का कोई प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं हुआ, यह अपवाद है।
ब्याल पास बस भए खरारी। स्वबस अनंत एक अबिकारी ।।
ऊपर का आधा चरण बताता है कि भगवान नागफाँस में बंध गये, यह अध्यारोप है और दूसरा चरण कहता है कि वे नहीं फँसे, क्योंकि वे स्ववश हैं, अनन्त हैं, एक हैं और अविकारी हैं, यह अपवाद है। प्रश्न होता है कि श्रुति यहाँ ऐसा और वहाँ वैसा क्यों कही? देखो -
पिता-पुत्र कहीं जा रहे थे, उनने दोपहर में विस्तृत सपाट मैदान में मृगजल देखा। पुत्र छोटा बालक था। मृगजल को देखकर उसने पिता से पूछा पिताजी! सामने यह जो नदी बह रही है वह कहाँ से निकली है? पिता ने सोचा कि यदि इसे सच-सच बताया जाय तो यह समझेगा नहीं, क्योंकि यह अभी अबोध है। नदी, पानी आदि कुछ नहीं है ऐसा कहने पर यह नहीं मानेगा, ऐसा सोच पिता ने कहा- बेटा विन्ध्याचल पर्वत पर बन्ध्या का एक पुत्र रहता है, उसने एक तालाब खुदवाया है, जिसमें असत्य का जल भरा है, वहीं से यह नदी निकली है। पुत्र छोटा बच्चा था, पिता की यह बात मान गया।
कुछ वर्ष बीतने पर जब पुत्र बड़ा हो गया तब एक बार फिर अपने पिता के साथ जाते हुए फिर मृगजल देखा, तब उसने फिर पिता से वही प्रश्न पूछा-तब पिता ने सोचा कि अब यदि वह पुरानी बात इससे कही जायगी, तब यह उसे मानेगा नहीं, क्योंकि इसकी बुद्धि अब समझने लग गयी है, इसलिए पिता ने कहा-बेटा! एक बार तुमने फिर यही प्रश्न किया था, तब हमने तुम्हें बताया था कि विन्ध्याचल पर्वत पर वन्ध्या का एक पुत्र रहता है। उसने एक तालाब खुदवाया है, जिसमें असत्य का जल भरा है वहीं से यह नदी निकली है। इस पर पुत्र कहने लगा कि वाह पिताजी! आप भी क्या गप्प हाँकते हो, क्या बन्ध्या का भी कहीं पुत्र होता है? तब पिता ने कहा नहीं। असत्य का भी कहीं जल होता है? पिता ने कहा नहीं। पुत्र ने कहा तब तालाब किसने खुदवाया? किसी ने नहीं। तब नदी कहाँ से निकली ? कहीं से नहीं। तब यह क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर पिता ने पुत्र को वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा-बेटा! जूते उतार दो। पुत्र ने जूते उतार दिये, तब उसका पैर तपी हुई भूमि पर जलने लग गया, छाले आ गये। पानी कहीं नहीं मिला। तब पिता ने सूर्य की ओर दिखाकर कहा कि यह सूर्य भगवान का चमत्कार है। रेत में सूर्य की किरणें पड़ने से ऐसा भास हो रहा है। पर, है कुछ भी नहीं। अभाव में भाव बताकर, सूर्य को अधिष्ठान बताकर, असत्य जल का अभाव समझाया। नदी का प्रवाह है ही नहीं बताया। जो कि वास्तविक था। पहिले जल का अभाव था, वहाँ जल का भाव अर्थात् होना बताया गया। इसे अध्यारोप कहते हैं और बाद में उसके कारण (अधिष्ठान) सूर्य को बताकर जल के भाव का अभाव कर दिया गया अर्थात् किये गये अध्यारोप का खण्डन कर दिया गया। इसको अपवाद कहते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए सन्त महात्माजन तथा वेद, शास्त्र निष्प्रपंच ब्रह्म में जगत् प्रपंच का अध्यारोप करते हैं और आगे चलकर स्व-स्वरूप भगवान आत्मा अधिष्ठान का ज्ञान कराकर किये गये अध्यारोप का खण्डन कर देते हैं। प्रपंच के अजातवाद से ईश्वर के कर्त्तव्य का अभाव है। अजातवाद का अर्थ है, जो तीनों काल में हुआ ही नहीं। संसार प्रपंच न कभी है, न हुआ है और न होगा।
सर्वप्रथम नारायण तत्त्व भगवान आत्मा में पहले जगत् की कल्पना हुई। इसके बाद उसके उत्पत्ति, पालन, संहार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कल्पना हुई। इसके बाद विषयों की कल्पना होते गयी। इस तरह संसार खड़ा हो गया।
बिना उपकरण के जो देखता है, उसको करते हैं उपद्रष्टा। अनुमान करने वाले का नाम अनुमन्ता है। सर्व का भरण-पोषण करता है, वह भर्ता है, वही जीव रूप से भोक्ता है। वही सर्व की आत्मा होने से परमात्मा है और शरीर के अन्दर उसी आत्मा को पुरुष कहते हैं। इस तरह 'मैं' आत्मा ही यह सब हुआ। अतः, 'मैं' ही स्वयं जगत प्रपंच हूँ। इसलिए माता कौशल्या कहती हैं कि -
देबि मोहबस सोचिअ बादी । बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी ।
भूपति जिअब मरब उर आनी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी ।
सीय मातु कह सत्य सुबानी । सुकृती अवधि अवधपति रानी ।।
महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी! हम अपने हित की हानि देखकर (स्वार्थवश) करती हैं। सीता जी की माता ने कहा-आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं की सीमा रूप अवधपति (महाराज दशरथ जी) की ही तो रानी हैं। (फिर भला, ऐसा क्यों न कहेंगी)
दोहा- लखनु रामु सिय जाहुँ बन भल परिनाम न पोचु ।
गहबरि हियँ कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु ।।
(अ.का. दो. 282)
कौशल्या जी ने दुःख भरे हृदय से कहा- श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वन में जायें, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है।
ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतबधू देवसरि बारी ।
राम सपथ मैं कीन्हि न काऊ। सो करि कहऊँ सखी सतिभाऊ ॥
ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे (चारों) पुत्र और (चारों) बहुएँ गंगाजी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी! मैंने कभी श्रीराम की सौगन्ध नहीं की, सो आज श्रीराम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ।
भरत सील गुन बिनय बड़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ।
कहत सारदहु कर मति हीचे । सागर सीप के जाहिं उलीचे ॥
भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वतीजी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप में कहीं समुद्र उलीचा जा सकता है।
जानउँ सदा भरत कुलदीपा । बार बार मोहि कहेउ महीपा ।।
कसें कनकु मनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिखिअहिं समर्यं सुभाएँ ।।
मैं भरत को सदा कुल दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार-बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी (जौहरी) से मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही (उसका चित्र देखकर) हो जाती है।
अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक सनेहैं सयानप थोरा ।
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी। भई सनेह बिकल सब रानी ।।
किन्तु, आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन (विवेक) कम हो जाता है। (लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ) कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह के मारे बिकल हो उठीं।
दोहा- कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देबि मिथिलेसि ।
को बिबेकनिधि बल्लभहिं तुम्हहि सकइ उपदेसि ।।
(अ.का.दो. 283)
कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा- हे देवी मिथिलेश्वरी! सुनिये, ज्ञान के भण्डार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है?
रानि राय सन अवसरू पाई । अपनी भाँति कहब समुझाई ।
रखिअहिं लखनु भरतु गवनहिं बन। जौं यह मत मानै महीप मन ।
हे रानी! मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहियेगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाय और भरत वन को जायँ। यदि, यह राय राजा के मन में (ठीक) जँच जाये।
तो भल जतनु करब सुबिचारी । मोरें सोचु भरत कर भारी ।।
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं । रहें नीक मोहि लागत नाहीं ॥
तो भली-भाँति खूब विचारकर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उसके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। सोच है। लगता है कि उसके प्राणों को कोई भय न हो जाये।)
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी। सब भइ मगन करुन रस रानी।
नभ प्रसून झरि धन्य-धन्य धुनि । सिथिल सनेहैं सिद्ध जोगी मुनि ।।
कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियाँ करुण रस में निमग्न हो गयीं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गयी और धन्य-धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गये।
सबु रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ । तब घरि धीर सुमित्रों कहेऊ ।
देबि दंड जुग जामिनि बीती । राम मातु सुनि उठी सप्रीती ॥
सारा रनिवास देखकर चकित (निःस्तब्ध) रह गयी। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरके कहा कि हे देवी! दो घड़ी रात बीत गयी है। यह सुनकर श्रीराम जी की माता कौशल्या जी प्रेमपूर्वक उठीं।
दोहा- बेगि पाउ घारिअ थलहि कह सनेहैं सतिभाय ।
हमरे तौ अब ईस गति कै मिथिलेस सहाय ।।284||
हमरें तौ अब ईश्वर की गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं।
लखि सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकप्रिया गह पाय पुनीता ।
देबि उचित असि बिनय तुम्हारी । दशरथ घरिनि राम महतारी ।।
कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी के प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिये और कहा- हे देवी! आप राजा दशरथ की रानी और श्रीरामजी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है।
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं । अगिनि घूम गिरि सिर तिनु घरहीं।
सेवकु राउ करम मन बानी । सदा सहाय महेसु भवानी ॥
प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएँ को और पर्वत तृण (घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं।
रउरे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै।
रामु जाइ बनु करि सुर काजू । अचल अवधपुर करिहहिं राजू ।।
आपका सहायक होने योग्य जगत् में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता कर जाकर कहीं शोभा पा सकता है?
श्रीरामचन्द्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे।
अमर नाग नर राम बाहुबल । सुख बसिहहिं अपने-अपने थल।
यह सब जागबलिक कहि राखा । देबि न होई मुधा मुनि भाषा ॥
देवता, नाग और मनुष्य तब श्रीरामचन्द्रजी की भुजाओं के बल पर अपने- अपने स्थलों (लोकों) में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी! मुनि का कथन व्यर्थ (झूठा) नहीं हो सकता।
दोहा- अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ ।
सिय समेत सिय मातु तब चली सुआयसु पाइ !!285||
ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़ कर सीता जी (के साथ भेजने) के लिए विनती करके और सुन्दर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। बस, यहीं पर रानियों की सभा एवं चित्रकूट दरबार की परिसमाप्ति है और यही राम दर्शन द्वितीय भाग का उपसंहार है।
राम अमित गुन सागर, थाह कि पावै कोय ।
संतन सन जस कछु सुनेउँ, तुमहिं सुनायेंउँ सोय ।।
तृतीय खण्ड़
1. वंदना एवं नाम महिमा
2. राम गीता पृष्ठ
3.विभीषण-शरणागति
4.वेद स्तुति पृष्ठ
5. राम राज्य की व्याख्या
6. ज्ञान भक्ति निरुपण
7.भगवान शंकर और माता पार्वती संवाद
1. नाम महिमा
।। श्री गणेशाय नमः ।।
।। श्री गुरुवे नमः ।।
नारायणोपनिषत्
ॐ अथ पुरुषो ह वै नाराणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति। नारायणात्प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योंतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणाद्ब्रह्म जायते। नारायणाद्रदो जायते। नारायणादिन्द्रो जायते। नारायणाव्प्रजापतिः प्रजायते। नारायणाद्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात्प्रवर्तन्ते। नारायणे प्रलीयन्ते। अर्थ नित्यो नारायणः। ब्रह्मा नारायणः। शिवश्च नारायणः। शक्रश्च नारायणः। कालश्च नारायणः। दिशश्च नारायणः विदिश्च नारायणः। ऊर्ध्वं च नारायणः। अधश्च नारायणः। अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्। निष्कलंको निरंजनो, निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुदेव भवति।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
रामाय राम भद्राय, रामचन्द्राय वेधसे।
रघुनाथाय नाथाय, सीतायाः पतये नमः ।।
यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा ।
यत्सत्त्वादममृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेभ्रमः ।।
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां ।
वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ।।
अनन्त नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्वेन प्रस्फुरित, महामहिम, स्वात्मस्वरूप सकल चराचर वृन्द एवं समुपस्थित आत्म जिज्ञासु गण 'उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत् ।
अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवो ! उठो ! स्व- स्वरूप भगवान आत्मा में जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर अपना आत्म कल्याण करो। मानव जीवन का यही चरम लक्ष्य है। यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवचन श्री रामचरित मानस के आधार पर हो रहा है।
अनन्त जिज्ञासुओं !
अनन्त जीवों के पूर्वार्जित पुण्य उदय होने पर एवं भगवान सच्चिदानन्द विश्वात्मा राम की असीम कृपा से ऐसा स्वर्ण अवसर श्री रामचरित मानस सुननेको मिलता है।
यह रामचरित मानस भारत वर्ष की अनुपम विभूति है। समस्त जीव मात्र के लिए संसार सागर से तरने के लिए यह परम नौका है। श्रद्धालु भक्तजन इसका नित्य पाट करते हैं। इसका विचार करते हैं, क्योंकि रामायण समस्त ज्ञान, विज्ञान और भक्ति का भंडार है। धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक सभी विषयों का इसमें ऐसे सुन्दर प्रसंग हैं कि बिना सन्तों की कृपा के ये समझ में नहीं आते। इसीलिए, तो मानसकार ने कहा है कि -
दोहा - श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम कै गूढ़ ।
किमि समुझौं मैं जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिमूढ़ ।।
(बा.का.दो 30-ख).
जब राम ही गूढ़ है, तब उनका चरित्र अर्थात् कथा तो गूढ़ होगी ही। जब तक जीव भाव का अभाव नहीं हो जाता, तब तक यह समझ में नहीं आता, इसीलिए ज्ञान निधि कहा गया।
अभी का प्रसंग है बालकाण्ड के अन्तर्गत "नाम महिमा" गोरखपुरी रामायण दोहा नं. 18वां से।
दोहा- गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न ।
बंदउँ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ||18||
गिरा कहते हैं वाणी को, अर्थ कहते हैं उस वाणी के मतलब को, बीचि कहते है लहर को। वाणी का अर्थ, श्लोक का अर्थ, शब्द का अर्थ अर्थात् वाणी अलग है और उसका अर्थ अलग है। श्लोक अलग है और उसका अर्थ अलग है, शब्द अलग है आ उसका अर्थ अलग है, इस तरह ये अलग-अलग हैं, भिन्न-भिन्न हैं, दो हैं, कहने। तो दो की प्रतीति होती है 'कहियत भिन्न' परन्तु 'न भिन्न' अर्थात् वे भिन्न-भिन्न ना है, वाणी ही अर्थ है, शब्द ही अर्थ है, जैसे 'जल बीचि सम'।
पानी की लहर कहने में पानी और लहर अलग-अलग जान पड़ते हैं, परन्तु 'न भिन्न'। अरे भाई! जल ही लहर है, लहर का आधार जल है, बिना जल के लहरों न किस पर? किसको लहर कहोगे? ऐसे ही वाणी का आधार अर्थ है, क्योंकि जसरी जिसकी सिद्धि होती है वह उससे भिन्न नहीं होता। सूत का वरत्र, सोने का आभूषण, लकड़ी का डण्डा, ये सब 'कहियत भिन्न' कहने में भिन्न-भिन्न है, ऐसा लगता है, परन्तु विचार कर देखो तो न भिन्न, अरे! सूत ही वस्त्र है, सोना ही आभूषण है, लकड़ी ही डण्डा है।
इसी तरह 'बन्दौ सीता राम पद' सीता राम, कहने में दो की प्रतीति होती है सीता और राम, परन्तु 'न भिन्न' वे अलग-अलग नहीं हैं। सीता, राम है और राम ही सीता है कहते हैं। परन्तु, विचारने से 'न भिन्न' माया ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही माया है। यदि माया की भिन्न सत्ता हो, बिना ब्रह्म के माया सिद्ध हो जाय, तब तो माया और ब्रह्म भिन्न-भिन्न हैं, दो हैं और यदि बिना ब्रह्म के माया सिद्ध नहीं होती तो ब्रह्म ही माया है, माया ही ब्रह्म है। राम और सीता, ब्रह्म और माया, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति कहते हैं स्वभाव को। स्वभाव, स्वभावी से भिन्न नहीं होता। जैसे-देखना आँख का स्वभाव है, आँख है स्वभावी और देखना है स्वभाव। तब यदि देखना न होगा तो आँख कहोगे किसको?
जिसका अर्थ नहीं होता उसे कहते हो, अरे! यह निरर्थक है। पुरुष और प्रकृति अर्थात् पुरुष ही प्रकृति है, प्रकृति ही पुरुष है। व्यवहारिक जगत् में कहा जाता है कि अरे भाई! छोड़ो, जाने दो, इनकी ऐसी प्रकृति ही है, आदत छूट सकती है, परन्तु प्रकृति याने स्वभाव बदला नहीं जा सकता, क्योंकि स्वभावी से स्वभाव भिन्न हो तब तो वह बदल जाये, परन्तु जब स्वभावी ही स्वभाव है, तब उसे बदल कैसे सकते हो? इसलिए प्रकृति जो है वह पुरुष का स्वभाव है। ब्रह्म, जगत्, जीव, ईश्वर, राम- सीता, भगवान और माया इनको स्वभाव और स्वभावी जानो, ये दो नहीं, एक ही है।
प्रश्न होता है-तब सिया राम, दो शब्द क्यों कहा गया?
उत्तर है- जहाँ तक वाणी का विषय है वह तो सीता और जिस आधार पर मन का विषय है वह है राम।
विषय समझो देखो संसार के प्रत्येक पदार्थ में पाँच अंश होते हैं- अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप।
देखो-यह फूल है, इसको कुछ मत मानो, फिर देखो, जैसे शिशु अर्थात् गोद का बच्चा (तीन-चार महीने की अवस्था) देखता है, उस स्तर से देखने पर यह फूल नहीं है, वह बालक यह नहीं जानता कि यह फूल है, परन्तु उसे यह कुछ प्रतीति तो हो रहा है, उसे कुछ भान तो हो रहा है उसकी दृष्टि में कुछ 'है'। तो, बस! यह जो है की प्रतीति हो रही है, वही अस्ति है, अस्तित्व है, 'है' है, यह जो अस्तित्व है वही सत् है, जो भास रहा है, उसकी प्रतीति होना भासना, यही चित् है, अर्थात् चेतन है और जो भास रहा है (चेतन) वही प्रिय है अर्थात् आनन्द स्वरूप है। इस तरह जिसे तुम फूल कह रहे हो, वह अस्ति, भाति, प्रिय अर्थात् आनन्द स्वरूप है। इस तरह जिसे तुम फूल कह रहे हो, वह अस्ति, भाति, प्रिय अर्थात् सत्, चित्, आनन्द अर्थात् सच्चिदानन्द राम हुआ यही तीन अंश राम है, अब इस अस्ति, भाति, प्रिय (सत, चित्, आनन्द) (सच्चिदानन्द) राम पर फूल की कल्पना की गयी, फूल का विकल्प हुआ, फूल माना गया, तब फूल यह नाम और इसका यह रूप जो दिखाई दे रहा है ये दो अंश (नाम और रूप) माया है, अर्थात् सीता है, क्योंकि मानना ही माया है। यदि, अस्ति, भाति, प्रिय यह आधार न हो, इसे यदि अलग कर लो तो फूल मानोगे किसको? फूल का नाम और यह रूप, किसके आधार पर रहेगा? गोद का बच्चा आगे चलकर उसी अस्ति, भाति, प्रिय को ही कहता है फूल है, अब उस फूल की मान्यता हुई, फूल का विकल्प हुआ, जो मान्यता ही सीता है। अब दृष्टि पसार कर देखो इस अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप से कोई खाली है? इस तरह जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है वह सब राम और सीता ही तो है, इसी स्थल पर मानसकार अपने अनुभव रख रहे हैं कि -
आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल थल नभ बासी।
सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥
चौरासी लाख योनियों में चार प्रकार के जीव (स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जरायुज) जल, थल और आकाश में रहते हैं, उन सबसे पूर्ण (भरे हुए) इस सारे जगत् को श्री सीता राम जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
इस तरह सारा चराचर राम और सीता ही है, उससे एक तृण भी खाली नहीं है।
बंदउँ सीता राम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न।
ये वाणी भी तो अस्ति, भाति, प्रिय पर ही अवलम्बित है, आधारित है। इल अनुभूति में अब कहाँ गया संसार? किसको तुम संसार कहते हो?
ये राम और सीता, जल और तरंग वत् एक-दूसरे से भिन्न नहीं है, जैसे जल से तरंग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अस्ति, भाति, प्रिय से, नाम और रूप अलग नहीं किया जा सकता। भगवान (राम) से माया (सीता) को अलग मानना यही दुःख का कारण है। माया तो भगवान का रक्षक है, राम बल्लभ है, सीता बल्लभा है, जो इनमें भेद डालता है, उन्हें अलग-अलग मानता है उसकी खैरियत कहाँ है? भाई! इसी में दुनिया पिसी जा रही है, जो भगवान और माया को भिन्न-भिन्न मानती है। माया बेचारी कितनी रक्षक है, जो भगवान को ढाँक-मूँदकर रखती है, वह अधिकारी को तो देखने देती है और अनधिकारी से छिपा लेती है उसे दर्शन नहीं कराती।
अधिकारी कौन? जो माया को राम ही जानता है, जिनकी दृष्टि में माया और भगवान दो नहीं हैं, एक ही है।
भगवान, माया से परे है, 'माया से परे है' कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान देश में माया है ही नहीं। दुनिया माया से विरोध करती है, इसलिए दुःख पाती है।
निज भ्रम नहिं समुझहिं अग्यानी। प्रभु पर मोह घरहिं जड़ प्रानी ।
जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ।।
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ।
उमा राम विषइक अस मोहा । नभ तम घूम घूरि जिमि सोहा ।।
(बा.का., शि.गी.)
संसार के जितने जीववादी हैं और यदि वे यहाँ बैठे हों तो उन्हें कहना है कि भाई! माया से यदि तरना चाहो तो माया से भगवान को भिन्न मत मानो, एक ही जानो।
यही गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद्, शास्त्रों एवं सन्त महात्माओं का तथा स्वयं हमारा अनुभव है। यदि फँसना है तो भगवान को माया मानो और यदि उससे छूटना है, निकलना है तो माया को भगवान जानो । भगवान कृष्ण कहते हैं -
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।
(गीता अ. 7, श्लोक 14)
आगे मानसकार अब केवल राम की वन्दना करते हैं.
बंदउँ नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को ।।
सन्त तुलसीदास कहते हैं कि भगवान रघुनाथ का जो श्रेष्ठ नाम राम है, उसकी मैं वन्दना करता हूँ, वह नाम कैसा है? तो कहते हैं-हेतु कृशानु कृशानु अर्थात् अग्नि, भानु अर्थात् सूर्य और हिमकर अर्थात् चन्द्रमा। हिमकर को
अग्निवंश में परशुराम का अवतार हुआ, सूर्यवंश में रामावतार और चन्द्रवंशक्ष बलरामावतार हुआ, अतः तीनों वंश के राम हेतु हैं, कारण है-
स्वांसा से सोहं हुआ, सोहं से ओंकार ।
ओंकार से रर्रा हुआ, साधू करौ विचार ।।
जो कुछ था, जो कुछ है, जो कुछ होगा, वे सब ओंकार ही है भाई! जिसको कु शरीर कहते हो वह साक्षात् भगवान ओंकार है, जिसका उच्चारण नहीं हो सकता वही तुम हो, अर्द्धमात्रा का क्या उच्चारण होगा? वह नित्य है। इसलिए,
बंदउँ नाम राम रघुबर को। हेतु कृशानु भानु हिमकर को ॥
बिधि हरिहर मय बेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥
वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव अर्थात् कल्याण स्वरूप हैं, वे वेदों के प्राण हैं, के उसकी ही व्याख्या करते हैं, वह अगुण हैं अर्थात् तीनों गुणों से रहित हैं, अस्ति भ्राति, प्रिय, रूप राम में टिको तो 'अगुण' अर्थात् तीनों गुणों से परे हो गया, वहाँ गुणों का क्या काम? वह तो गुणातीत पद है, वह अनुपम है, उसके समान दूलर नहीं, जब दूसरा हो तब उपमा दी जाय। वह सर्वगुणों का भण्डार है। सर्व गुण उसे पर आधारित है।
महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥
भगवान शंकर 'राम' इस महामंत्र का दिन-रात जप करते रहते हैं। कहा जात है कि जो काशी में मरते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, ऐसी कहावत है, इसका तात्प यह है कि "काशः ब्रह्म प्रकाशः यस्यां अवस्थायां सा काशी" वही काय मरणान्मुक्ति। अर्थात् जिस अवस्था में हृदय में ब्रह्म का प्रकाश हो जाये वही काश।। और उसी काशी में मरने से मुक्ति होती है।
महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥
जिस राम नाम की महिमा को गणराऊ गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहिले पूजे जाते हैं, जिसकी कथा तो जानते ही हो, अरे! जो सबका ईश हो उसे कहते हैं "गणेश'।
गणानां ईशः गणेशः, देवानां ईशः देवेशः ।
जान आदिकबि नाम प्रतापू । भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ।।
आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उलटा नाम जपकर पवित्र हो गये, तो भाई! उलटोगे तब तो शुद्ध होगे, उलटना क्या?
जग से छत्तीस रह, राम चरण छः तीन ।।
संसार की ओर से उलटकर, राम की ओर मुँह कर लो।
सहस नाम सम सुनि सिवबानी। जपि जेई पिय संग भवानी ।।
माता पार्वती जी शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, वे सदा अपने पति भगवान शंकर के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं -
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ।।
हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को ।
नाम प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फलु दीन्ह अमी को ।।
नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिवजी हर्षित हो गये और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया अर्थात् उन्हें अपने अंग में धारण कर अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिवजी भली-भाँति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उन्हें अमृत का फल दिया।
दोहा - बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास ।
राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास ।।
(बा.कां. दो. 19)
भगवान राम की भगति वर्षा ऋतु है, जितने भक्तगण हैं, वे धान के फसल हैं, और 'र' और 'म' ये दोनों अक्षर सावन भादों के महीने हैं।
आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ।
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहु परलोक निबाहू ।।
दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, ये मधुर नाम लोक और परलोक दोनों को सम्भालने वाले हैं।
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ।
बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती ॥
ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुन्दर और मधुर हैं, तुलसीदास को 'र' और 'म' ये दोनो राम और लक्ष्मण के समान अत्यन्त प्यारे हैं, इनके अर्थ और फल में जरा भी भिन्नता नहीं है। ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही सदा एक रस और एक रूप हैं। इससे स्पष्ट है कि जीव और ब्रह्म दोनों अलग-अलग नहीं, वरन स्वभाव से ही एक ही हैं।
नर नारायन सरिस सुभ्राता । जग पालक बिसेषि जन त्राता ।
भगति सुतिय कल करन विभूषन । जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन ।।
ये दोनों अक्षर 'रा' और 'म' नर-नारायण के समान सुन्दर भाई हैं, ये जगत् का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपिणी सुन्दर स्त्री के कानों के आभूषण सुन्दर कर्णफूल हैं और जगत् के हित के लिए निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं।
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ सेष सम घर बसुधा के ।
जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलधर से ।।
इनमें मोक्ष रूपी अमृत का स्वाद भरा है, ये कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। ये भक्तों के मन रूपी सुन्दर कमल में बिहार करने वाले भौरों के समान हैं और जीभ रूपी यशोदाजी के लिए श्रीकृष्ण और बलराम के समान आनन्द देने वाले हैं।
दोहा - एकु छत्र एकु मुकुटमनि, सब बरननि पर जोउ।
तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दोउ ||20।।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक "रकार" छत्ररूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है।
समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ।
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥
समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किन्तु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, नाम और नामी दोनों एक-दूसरे से अभिन्न हैं, दोनों में ऐसी एकता है कि नाम के पीछे नामी चला करता है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं, ये दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, परन्तु भैय्या! जिसकी निर्मल भक्ति परि पूरित पवित्र बुद्धि होगी, उस बुद्धि से ही, इसका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। अस्ति, भाति, प्रिय, भगवान राम है और नाम रूप, भगवान राम की उपाधि है। वास्तविकता पर जो पर्दा डाले उसे उपाधि कहते हैं।
भगवान के छिपने की झाड़ी माया है। नाम रूप ही माया है। परन्तु, जब मायापति अकथ है, तब माया भी अकथ ही है। अधिष्ठान में कल्पित धातु, अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती बिना अधिष्ठान, परम तत्त्व भगवान आत्मा के नाम रूप (माया) किसके आधार पर रहेंगे? जैसे, लकड़ी से डण्डा भिन्न नहीं, मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं, सूत से वस्त्र भिन्न नहीं, जब यह अटल नियम है कि अधिष्ठान से भिन्न उसमें कल्पित वस्तु नहीं होती, तब मुझ आत्मा राम में नाम रूप जो कल्पित है वह उससे भिन्न कैसे हो सकती है। इसलिए, माया भी अकथनीय है, अनादि है, परन्तु अनन्त नहीं है, माया के अस्तित्व के अज्ञान से ही माया है, इसलिए अधिष्ठान के ज्ञान हो जाने पर माया शांत हो जाती है। जब तक अधिष्ठान को नहीं जाना, तभी तक माया है, जब अधिष्टान का ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, दर्शन हो गया, तब माया न रही, अधिष्ठान का अधिष्ठान ही रह गया, लकड़ी के बोध हो जाने पर उस पर कल्पित डण्डा न रहा, लकड़ी ही रह गयी। ऐसे ही भगवान 'मैं' राम अधिष्ठान पर जगत् प्रपंच, माया, जो कल्पित है, वह 'मैं' आत्मा के बोध हो जाने पर शांत हो जाती है। मतलब यह है कि 'मैं' आत्मा राम ही हूँ, जिसका नाम माया है।
को बड़ छोट कहत अपराधू । सुनि गुन भेदु समुझिहहिं साधू ।
देखिअहिं रूप नाम आधीना। रुप ग्यान नहिं नाम बिहीना ।।
इसमें से किसी को छोटा और किसी को बड़ा कह कर कौन अपराध मोल ले "नाम रूप गति अकथ कहानी" इसकी गति अकथ है, मान्यता ही माया है, मानता कौन है? किसको मानता है? ये सब समझने की चीज है, बखान करने की नहीं।
जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग्विधान् ।
बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथाविद्यस्तथास्मृतिः ॥
(मांडू उ.वै.प्र.मं-16)
सबसे पहिले परमात्मा ने अपने आप को ही माना कि 'मैं' संसारी जीव हूँ। अब विचार करो कि 'मैं' जीव हूँ, इस वाक्य में हूँ क्रिया किसकी है, 'मैं' की या जीव की? अगर हूँ क्रिया जीव की है, तब तो मैं जीव हूँ और यदि हूँ क्रिया 'मैं' की है, तो 'मैं' जीव नहीं हूँ, भगवान ही हूँ। यह अकुंठित सिद्धान्त है, सारे विश्व के जीववादियों के लिए यह चुनौती है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, देव हों या दैत्य हों, कोई भी हों, अखिल ब्रह्माण्ड के जीव वादियों का कहना है कि 'हूँ' क्रिया 'मैं' की है, जीव की नहीं।
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ।।
गुणातीत ब्रह्म और साकार ब्रह्म, निर्गुण और सगुण दोनों का यह सुसाखी है अर्थात् चतुर दुभाषिया है (दो भाषाओं के जानने वाले को दुभाषिया कहते हैं) यह राम नाम जो है वह सगुण है और निर्गुण दोनों का ज्ञान कराता है।
दोहा - राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरीं द्वार ।
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहसि उजिआर ||21||
भाई! अगर बाहर और भीतर दोनों जगह उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि को जिह्वा रूपी देहरी द्वार पर रखो। बाहर अन्धकार है, जिसके कारण रामसीय मय सारा चराचर भगवान भास, संसार दिखाई दे रहा है और भीतर के अंधकार के कारण भगवान आत्मा 'मैं' जीव दिखाई दे रहा है। दिन-रात, तबला मजीरा के साथ गा रहे हो कि -
सीय राम मय सब जग जानी।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानि ॥
परन्तु हृदय में वैसी धारणा क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि तुम्हारा गाना बजाना भी अंधेरे में ही हो रहा है, बाहर-भीतर दोनों जगह अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार के कारण ही सत को असत्, जड को चेतन, अंधकार को प्रकाश दुनिया मानते चली आ रही है। अब प्रश्न होता है कि हम तो रोज हजारों माला सरका-सरका कर जीभ से राम नाम का जप कर रहे हैं, तब भी एक भी जगह प्रकाश नहीं हो पाया, जैसे पहले थे, वही अभी भी बने हुए हैं, इसका क्या कारण है? बाहर, भीतर अंधकार ही छाया हुआ है, प्रकाश न हो पाया।
इसका कारण यह है कि राम नाम मणि जीह देहरी द्वार पर नहीं रखा गया। मानसकार का भाव जिस देहरी द्वार से है उसे तो सन्त ही अनुभवी महान पुरुष ही उसे लखाते हैं। जानते हैं और सन्त
'भाई! विषय समझो -मानसकार का तात्पर्य जिसे तुम जीभ समझे हुए हो उस जीभ से नहीं, इस जीभ की जड़ में जहाँ से कि यह रस लेने वाली जीभ शुरू होता है वहाँ ही इस जीभ के ऊपर एक छोटी जीभ है, जिसे जीभी या काकल जिगुरू होती है। उस जीभ का अनुभव करो और उसी अन्तर्जिह्वा से राम नाम जपो, जप करत हम धीमी गति से हो, आराम से स्थिरतापूर्वक, निष्ठा और लगन के साथ, इस तरह काम जप करने से थोड़े ही काल में उस अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति होती है या नहीं इसका अनुभव करो, यही अन्तर्जिह्वा ही देहरी द्वार है जहाँ पर राम नाम मणि रखने से दोनों जगह बाहर और भीतर प्रकाशित होता है। यह गोपनीय रहस्य है, जिसे अधिकारी को ही बताया जा सकता है, परन्तु हमारी दृष्टि में सारा प्राणि मात्र ही जब अधिकारी है (क्योंकि सब की तलाश उसी नित्यानन्द की है) तब दुराव की गुंजाइश कहाँ है? दूसरी बात यह है कि कैसा भी गोपनीय रहस्य हो तुम लाखों लोगों के समक्ष प्रगट कर दो, परन्तु भैय्या! जो अधिकारी होता है, वही इसे पकड़ पाता है, सुनते सब हैं।
अब प्रसंग पर आ जाओ-प्रपंच को निष्प्रपंच करने के लिए, इस जीभ से जप करने पर मन अपने आप निर्विकल्प हो जाता है, फिर बाहर और भीतर दोनों प्रकाशित हो जाता है। बाहर जब प्रकाशित होता है तब जिसे तुम संसार कहते हो, जो तुम्हें संसार दिख रहा है वह भगवान दिखने लगता है, उस पर से जगत् भाव चला जाता है और भीतर जब प्रकाशित होता है तब 'मैं' पर अनादिकाल से देहभाव, जीवभाव आदि जो अमुक भाव है उसका सर्वथा अभाव हो जाता है और शुद्ध तत्त्व भगवान आत्मा 'मैं' का अनुभव होता है। यह एक ऐसा दीपक है कि जो स्वाभाविक है, इसीलिए इसे मणि की उपमा दी गई थी। अज्ञान अंधकार के मिटते ही, निर्विकल्पता की स्थिति में जगत्भाव और जीवभाव के अभाव होते ही सर्वभावों का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब इस स्थिति में जबकि देहभाव, जीवभाव, ब्रह्मभाव, जगतभाव, पुरुषभाव, प्रकृति भाव, सगुणभाव, निर्गुणभाव आदि कुछ भाव न रहा तब जो शेष रह जाता है, वह अनिर्वचनीय आनन्द (ब्रह्म सुख) अनुभव का विषय है उसे तो अनुभव करके ही जानोगे, वह कहने सुनने की चीज नहीं बल्कि अनुभव की वस्तु है।
नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी ।
ब्रह्मसुखहिं अनुभवहिं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ।।
इस विधि से नाम का जप करके योगी जागते हैं, कैसे योगी? अरे! जिसे ब्रह्मा के बनाये हुए इस प्रपंच से भली प्रकार से वैराग्य हो गया है ऐसे योगी, फिर वे ही इस ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। वह ब्रह्म सुख कैसा है? तो मानसकार कहते हैं कि 'अनूपा' और फिर 'अकथ' 'अनामय' फिर 'नाम न रूपा'। उस सुख की उपमा विश्व के किसी सुख से नहीं दी जा सकती, वह अकथ है, वह ब्रह्म सुख अपने से भिन्न हो तब तो वाणी उसे व्यक्त करे, क्योंकि अमुक भाव ही वाणी, बुद्धि, चित्त, इन्दियाँ आदि का विषय है, परन्तु जब सर्व अमुक भाव का ही अभाव हो गया तब मन, बुद्धि, चित्त इन्द्रियाँ वाणी आदि कहाँ रही, क्योंकि ये भी तो सब अमुक भाव ही है, तब फिर बतावैं कौन कि वह ब्रह्म सुख कैसा है? इसलिए अकथ।
वह अनामय अर्थात् मलरहित है। अरे, अमुक भाव हो तो मल है, जिसका वहाँ सर्वथा अभाव है। फिर उस अनिर्वचनीय आनन्द का न कोई नाम है और न रूप है वह केवल अनुभव गम्य है। इस जन्म में जपा और वह ब्रह्म सुख अगले जन्म में प्राप्त होगा। भैय्या, ऐसी बात नहीं है, तत्काल अनुभव करो, हाथ कंगन को आरसी क्या? यह तो नेशनल बैंक का चेक है, जहाँ चाहे वहाँ भुना लो।
एहि जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ।।
अज्ञान अंधकार में सोया था यही रात्रि थी, जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, तब अज्ञान रात्रि का अंत हो गया। तब सोना कहाँ? जागना ही जागना है।
जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ । नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ ॥
यदि नाम की गूढ़ गति को जानना हो तो इसी जीभ से नाम जपकर जाना जा सकता है, इस जीभ से जप करने पर जब निर्विकल्पता आ गयी तब संसार ही न रहा, सब बह गया, केवल अपना आप ही रह गया। अरे, यही तो नाम की गूढ़ गति है और यही भव सागर से तरना है।
जासु नाम सुमिरत इकबारा । उत्तरहिं नर भव सिन्धु अपारा ॥
बहुबारा नहीं, एक ही बार कहा गया, परन्तु इसी प्रकार सुमिरन करने कहा गया।
प्रश्न होता है-गूढ़ गति क्या है?
उत्तर है-अन्तर्जिह्वा से जप करने से, जिसका लक्षण गूढ़ है, जिसका अनुभव गूढ़ है, जप गूढ़ है, जो हर एक के वश की बात नहीं है, क्योंकि 'अकथ, अनामय, नाम न रूपा' है, तब वह गूढ़ नहीं तो क्या है? जो सर्व में, सर्वरूप से, सर्व होकर, सर्व का सब कुछ होकर है। इसलिए, वह गूढ़ नहीं तो क्या है? उसको जानना, अनुभव करना, समझना सभी गूढ़ है, बिना सन्त शरण के उसकी गूढ़ता कोई जान नहीं सकता। इसे तो वही जान पाता है, जिस पर सन्त भगवान की कृपा हो जाती है, जिसे सन्त शरण की उपलब्धि हो जाती है।
भगवान आत्मा 'मैं' प्रगट होते हुए गुप्त है और कठिन होते हुए सरल है, गुप्त होते हुए प्रगट है और सरल होते हुए कठिन है, यही भगवान आत्मा की गूढ़ता है। श्रुतियों, स्मृतियों, वेद, शास्त्रों और सन्त महात्माओं का कहना है कि वह भगवान आत्मा, मनवाणी का विषय नहीं है। प्रश्न होता है-क्यों?
उत्तर है अरे! जो मन का मन है, बुद्धि की बुद्धि है, चित्त का चित्त है, वाणी की वाणी है, इन्द्रियों की इन्द्रियाँ हैं तो फिर ये उसे क्या जान सकते हैं, अगर इनसे भिन्न हों, तब तो देखें, जाने और जब सर्व में सर्वरूप से, सर्व होकर सर्व का सब कुछ होकर है तो किसकी ताकत है कि उसे ढूँढ़कर निकाल ले, वह सामान्य रूप से सबमें घुला-मिला है तब फिर वह जाना कैसे जा सकता है? यही उसकी गूढ़ता है, यही गूढ़गति है, जिसका जानना, समझना, प्राप्त करना सब कुछ सन्त शरण की देन है, फिर तो वह गुप्त होते हुए प्रगट और कठिन होते हुए सरलतम है।
साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ।।
लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादिक सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं, परन्तु यह साधकों को ही मुबारक हो, भक्त इस ओर ध्यान भी नहीं देते क्योंकि - ये सब राम भक्ति के बाधक हैं।
अष्ट सिद्धि नव निद्धि को, साधू मारत लात ।।
सिद्धियाँ आठ हैं -
1. अणिमा सिद्धि - अत्यन्त छोटा हो जाना। मसक समान रूप कपि घरी
2. महिमा सिद्धि- आकाश तक बढ़ जाना, बड़ा हो जाना।
जस-जस सुरसा बदनु बढावा, तासु दून कपि रूप दिखावा ।।
3. लघिमा - अत्यंत सूक्ष्म हो जाना।
4. गरिमा सिद्धि - बहुत वजनीय हो जाना।
5. प्राप्ति सिद्धि - इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेना।
6. प्रकाम्य - कामनाओं की पूर्ति कर लेना।
7. वशीकरण - जिसे चाहे, वश में कर लेना।
8. ईशा - ईशवरता अर्थात् सब पर शासन करना।
इन आठ सिद्धियों की ही तरह नव निधियाँ भी हैं, परन्तु क्या करोगे। इन्हें सब जानकर आत्म कल्याण के लिए ये सब बाधक हैं। इसीलिए हम इन पर कभी रोशनी नहीं डालते।
आये थे हरि भजन को । ओटन लगे कपास ॥
हाँ, भगवान आत्मा को प्राप्त कर लो, फिर तो ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ तुम्हारे पीछ-पीछे फिरेंगी।
एक बार कोई सिद्ध महात्मा स्वामी राम के पास पहुँचे, व्यवहारिक शिष्टाचार के बाद स्वामी जी ने उन्हें बड़े प्रेम से अपने पास बिठाया और कुशल समाचार पूछने लगे। महात्मा सिद्ध थे, सनक में आकर वे कहने लगे स्वामी जी ! मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है, तब स्वामी राम ने पूछा भैय्या! वह कौन-सी सिद्धि है, जिसे तुमने प्राप्त किया है? महात्मा कहने लगे स्वामी जी। जैसे मनुष्य जमीन पर चलता है उसी प्रकार में पानी के ऊपर चल सकता हूँ, मेरा कोई अंग भींगने नहीं पाता, बढ़ी हुई नदी पार करने के लिए यह बड़ा लाभप्रद है, तब स्वामी राम ने कहा- भाई ! यह सिद्धी आपको कितने दिनों में प्राप्त हुई? महात्मा कहने लगे, महाराज! पूरे बारह वर्ष के कठिन तपस्या के बाद मैं इसे प्राप्त कर पाया हूँ। इस पर स्वामी जी कहने लगे-भाई! लोग नाविक को चार पैसे देकर नाव द्वारा बिना प्रयास नदी पार कर लेते हैं उसके लिए बारह वर्ष तक आपको कठिन तपस्या करनी पड़ी, आपने बड़ा कष्ट सहन किया और महत्वहीन चीज हासिल की इसी लगन से इतने काल तक यदि भगवत भजन हुआ होता तो जीवन कृतार्थ हो जाता।
एक बार इनके पास एक और अन्य महात्मा आए और वे कहने लगे, स्वामी जी! लोट-पोट कर देता है। तब स्वामी राम कहने सगे भाई! वेदान्त में वह ताकत है कि संसार तीन काल में है ही नहीं, इसे वह प्रत्यक्ष जोग में वह ताकत दिखा देता है तब लोटपोट किसको कराना।
जपहिं नामु जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ।।॥
संकट से घबराये हुए आर्त्त भक्त जन नाम जप करके कठिन से कठिन आपत्तियों नेछुटकारा पा जाते हैं। गजेन्द्र का ग्राह से छूटकारा पाना और कौरव सभा में द्रौपदी की लज्जा की रक्षा होना, ऐसे अनेक प्रमाण हैं।
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा ।।
संसार में चार प्रकार के भक्त हैं
1. अर्थार्थी - धन आदि की चाह से भजने वाले।
2. आर्त्त- दुःखों से छुटकारा पाने के लिए भजने वाले।
3. जिज्ञासु-भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले।
4. ज्ञानी - भगवान को तत्त्व से जानकर, स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। ये चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं।
चहू चतुर कहुँ नाम अधारा । ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा ।।
चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, इसमें ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष रूप से प्रिय हैं।
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ।।
यों तो चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, परन्तु कलियुग में विशेष रूप से इस युग में तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है, परन्तु श्रद्धा और विश्वास के बिना व्यक्ति रामखुदैय्या में पड़ जाता है, तो विफलता का कारण होता है।
किसी नगर के एक मुहल्ले में एक पंडित जी और एक मुल्लाजी पास-पास रहा करते थे। एक दिन इन दोनों में धार्मिक विवाद छिड़ गया। पंडित जी अपने राम की महिमा बताकर मुल्लाजी से कहते कि हमारा राम ही सब कुछ है, उनकी श्रेष्ठता के सामने तुम्हारे खुदा की क्या गिनती। मुल्लाजी इसका विरोध करते और कहते कि हमारे ख़ुदा के द्वारा ही संसार संचालित हो रहा है, हमारे ख़ुदा के अस्तित्व पर ही तुम्हारा राम टिका हुआ है, नहीं तो तुम्हारा राम किस खेत की मूली है।
इसी प्रकार विवाद बढ़ता गया, पंडितजी अपने राम की अपेक्षा खुदा को श्रेष्ठ मानना स्वीकार नहीं करते थे और मुल्लाजी अपने ख़ुदा की तुलना में राम की तुच्छता में यह तय हुआ कि राम और अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा की जाय।
पंडित जी ने कहा- देखो, सामने यह पीपल का बड़ा वृक्ष है, इसकी सबसे ऊँची चोटी पर चढ़कर अपने-अपने इष्ट का नाम लेकर नीचे जमीन पर कूदा जाय, जिसका इष्ट अधिक शक्तिशाली होगा वह अपने उपासक को बचा लेगा। मुल्लाजी ने शर्त माम ली, परन्तु पहिले पंडित जी ही झाड़ पर ऊपर चढकर नीचे कूदें यह बात सामने रखी गयी। पंडित जी को अपने राम पर पूर्ण विश्वास था, उसने मन में निश्चय किया कि जिस प्रभु ने ग्राह से गज की, दुश्शासन के अत्याचार से द्रौपदी की, दुर्योधन की दुष्टता से पाण्डवों की, हिरण्यकश्यप की क्रूरता से प्रहलाद की और राक्षसों की नीचता से देवताओं की हमेशा रक्षा की, क्या वे मेरी रक्षा करेंगे? अवश्य करेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं, ऐसा मन में ठान बड़ी श्रद्धा से भगवान का ध्यान कर अपनी धोती कस ली और पीपल के झाड़ की ऊँची चोटी पर चढ़ गये, मुल्लाजी मुँह बाँये ऊपर देखते रहे। पंडित जी ऊपर चढ़कर "जै भगवान राम की' कहकर धड़ाम से नीचे कूद पड़े। अपने राम पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होने के कारण नीचे कूदने पर पंडित जी को ऐसा अनुभव हुआ मानो वे रुई के ढेर पर कूदे हों। कहीं किसी अंग पर बल तक नहीं पड़ा, मुल्लाजी यह देखकर दंग रह गये।
अब मुल्लाजी के कूदने की पारी आयी, वे बड़ी चिंता में पड़े हुए झाड़ पर ऊपर चढने लगे, ऊपर चढ़कर मुल्लाजी ने विचार किया कि मैंने अपने ख़ुदा की कभी जीवन में परीक्षा नहीं ली, मालूम नहीं मुझे बचा सकने की शक्ति उनमें है या नहीं, परन्तु इनके राम की महिमा तो मैंने अपनी आँखों से अभी ही देख लिया हो सकता है इनके राम ही अधिक बलवान हों, परन्तु क्या हमारे ख़ुदा भी इतने कमजोर होंगे। इसी तरह दुविधा में पड़े हुए मुल्लाजी ऊपर डगाल पर बैठे हुए चिंता में डूब गये और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए।
जब मुल्लाजी को इसी सोच विचार में डगाल पर बैठे बडी देर हो गयी तब नीचे से पंडित जी ने ललकारा वहाँ डगाल पर कब तक बैठे रहोगे ? नीचे कूदो। मुल्लाजी को अब नीचे कूदना तो था ही उनने मन में सोचा कि राम और ख़ुदा दोनों का नाम लेका कूदा जाय जो अधिक शक्तिशाली होंगे वही मुझे बचा लेंगे, ऐसा निश्चय कर उनके राम और खुदा इन दोनों नाम को मिला एक नया नाम रामखुदैय्या बनाया और जै रामखुदैय्या की कहकर नीचे कूद पड़े। इनका दोनों में से एक पर भी पूर्ण विश्वास ही था। अतः, परिणाम यह हुआ कि नीचे कूदते ही इनकी हड्डी-पसली चूर-चूर नेमयी और मुल्लाजी वहीं ढेर हो गये। भाई! खुदा कहो चाहे राम कहो, दोनों एक ही वरमात्मा के भिन्न-भिन्न नाम हैं, तत्त्व एक ही है, आवश्यकता है इनमें पूर्णनिष्ठा, सच्ची श्रद्धा और अटल विश्वास के होने की. फिर तो वह सर्वत्र, समान और व्यापक बाहे जहाँ जिस क्षण प्रगट किये जा सकते हैं, भगवान शंकर कहते हैं -
हरि ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना ।।
कण-कण, जर्रा-जर्रा, भगवान है, खुदा है, उससे एक तिल भर भी जगह जानी नहीं है, खुदा या परमात्मा किसी एक जगह ही हो ऐसी बात नहीं है।
गर, ख़ुदा काबे में होता है तो बुतखाने में कौन ?
हर है गंगाजल में तो, जम-जम के पैमाने में कौन ?
ले चले मजनूं को जंगल, उसने हँसकर यूँ कहा,
लैला गर बस्ती में होती, है तो बीराने में कौन ?
दार पर मंसूर चढ़ा पर न समझा यह कोई,
था अनलहक कह रहा, मंसूर दीवाने में कौन ?
किससे बातें कर रहा है मुझको ऐ जाहिद बता,
छुपके बैठा है तेरी, तसबीह के दाने में कौन ?
अब आ जाओ प्रसंग पर -
दोहा- सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन ।
नाम सुप्रेम पियूष हृद। तिन्हहुँ किये मन मीन ||22|।
जो सब प्रकार के कामनाओं से रहित हैं और नित्य राम भक्ति का पीयूष पीते रहते हैं ऐसे भक्त जन भी नाम के सुन्दर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखे हैं, अर्थात् वे भी नाम रूपी सुधा का निरन्तर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते।
अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ।।
मोरें मत बड़ नामु दुहू ते। किए जेहिं जुग निज बस निजबूते ॥
निर्गुण और सगुण ये ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मानसकार करते हैं कि मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को वश में कर रखा है।
प्रौढ़ि सुजन जनि जानहिं जनकी। कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की।
एकु दारुगत देखिअ एकू । पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू ।।
उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम तें ।
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनंद रासी ।।
मानसकार कहते हैं कि सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रूचि की बात कहता हूँ कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है, निर्गुण उस गुप्त अग्नि के समान है, जो काठ के अन्दर है, परन्तु दिखती नहीं और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है, जो प्रत्यक्ष दिखती है परन्तु तत्त्वतः एक ही हैं, फिर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परन्तु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं, इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनन्द की घन राशि है।
अस प्रभु हृदयें अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी।
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥
ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत् के सब जीव, दीन और दुःखी हैं।
या जग दुखिया कोउ नहीं, सबकी गठरी लाल ।
गाँठ खोल जानें नहीं, तातें भइ कंगाल ।।
नाम के यथार्थ, महिमा, रहस्य और प्रभाव को न जानने से ही ऐसी दशा हुई है और उसके ज्ञान हो जाने पर वही ब्रह्म ऐसे प्रगट हो जाता है जैसे पास में रखे रत्ना पहिचान लेने पर उसका मूल्य।
दोहा - निरगुन ते एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार ।
कहउँ नामु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार ।।23।।
निर्गुण ब्रह्म से नाम का प्रभाव पड़ा है, परन्तु सगुण राम से भी मैं नाम को ब समझता हूँ, क्योंकि -
राम भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ।
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगल बासा ।।
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥
रिषि हित राम सुकेतुसुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ।।
सहित दोष दुख दास दुरासा । दलइ नामु जिमि रबि निसि नासा ॥
भंजेउ राम आपु भव चापू । भव भय भंजन नाम प्रतापू ।।
दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन ॥
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामु सकल कलि कलुष निकंदन ॥
दोहा- सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ ।
नाम उघारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ ||24||
भगवान राम ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके, स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को सुखी किया, परन्तु नाम ने तो अपने प्रभाव से अनेकों नाम प्रेमी भक्तों का उद्धार कर दिया। राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहल्या का ही उद्धार किया, परन्तु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया।
राम ने तो एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और सुबाहु की समाप्ति की, परन्तु नाम ने अपने अनेक प्रेमी भक्तों के दोष, दुःख और दुराशाओं का नाश किया।
राम ने दण्डक वन को सुहावना बनाया, परन्तु नाम ने असंख्य भक्तों के मनों को पवित्र कर दिया।
राम ने राक्षसों के सारे पापों की जड़ को उखाड़ फेंका। कहाँ तक कहें - राम ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परन्तु नाम ने अगणित दुष्टों का संहार किया, जिसकी कथा वेदों में अंकित है।
राम सुकंठ बिभीषन दोऊ । राखे सरन जान सबु कोऊ ।
नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद बर बिरिद बिराजे ॥
राम भालु कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा ।
नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु बिचारु सुजन मन माहीं ।।
राम ने तो सुग्रीव और विभीषण दो को ही शरण दी, परन्तु नाम ने अनेक गरीबो पर कृपा की, जिसका वेद साक्षी है।
राम ने भालू और बन्दरों की सेना बटोरी और बहुत परिश्रम से समुद्र में पुल बाँधने के बाद समुद्र को पार किया, परन्तु यहाँ? नाम लेते ही संसार सागर सूब जाता है, परन्तु विचार करो तब, अन्यथा नहीं।
राम सकुल रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा।
राजा रामु अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनिबर बानी ॥
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती । बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती।
फिरत सनेहैं मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥
राम ने कुटुम्ब सहित रावण को युद्ध में मारा तब सीता सहित अपने अयोध्याम प्रवेश किया, फिर राजा राम हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुन्दर वाणी से उनका गुण गाते हैं, परन्तु नाम प्रेमी भक्त प्रेमपूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते रहते हैं। नाम के प्रभाव से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती।
दोहा - ब्रह्म राम ते नामु बड़ बर दायक बर दानि ।
रामचरित सत कोटि महें, लिय महेस जियँ जानि ||25||
भाई! इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम इन दोनों से नाम बड़ा है, यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। भगवान शंकर ने इसका रहस्य समझकर ही, सौ करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को ही सार रूप में चुनकर अपने हृदय में ग्रहण किया है।
नाम प्रसाद संभु अबिनासी । साजु अमंगल मंगल रासी ।
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ।
नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू।
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥
नाम के ही प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। शुकदेव, सनकादि, सिद्ध मुनि, योगीगण, नाम के ही प्रसाद ब्रह्मानन्द को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना, इसलिए वे हरि को औ हर को दोनों को प्यारे हैं। नाम के प्रभाव से ही प्रह्लाद भक्त शिरोमणि हुए।
धुर्वे सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायउ अचल अनूपम ठाऊँ।
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू ।।
ध्रुव ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुःखी होकर सकाम भाव से नाम जप किया और उसके प्रताप से अचल, अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्रीराम को ही अपने वश में कर रखा है।
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ।
कहाँ कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई ।।
नीच अजामिल, गज, गणिका (वेश्या) भी नाम के ही प्रभाव से, तर गये, मुक्त हो गये। अरे! मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूँ, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते।
दोहा- नामु राम को कलपतरु, कलि कल्यान निवासु ।
जो सुमिरत भयो भाँगते, तुलसी तुलसीदासु ||26||
कलियुग में राम का नाम कल्पतरु के समान कल्याणप्रद है, जिसका स्मरण करने से ही भाँग के समान (निष्कृष्ट), तुलसीदास, तुलसी के समान पवित्र हो गया।
भैया! राम नाम की महिमा अनन्त है, कहाँ तक कहा जाये -
भायें कुभायें अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ।।
अच्छे भाव से, बुरे भाव से, बैरभाव से, आलस्य भाव से, किसी भी भाव से हो, नाम जपने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और उसे दसों दिशाओं से आनन्द ही आनन्द की अनुभूति होती है। भाव से भजा विभीषण ने, कुभाव से भजा रावण ने, अनख से भजा बाली ने, आलस्य से भजा कुम्भकरण ने, इन सबका उद्धार हो गया, ऐसे ही काम से भजा गोपियों ने, क्रोध से भजा शिशुपाल, दन्तवक्र ने, भय से भजा कंस ने, एकता से भजा उद्धव ने, स्नेह से भजा वसुदेव-देवकी ने, वात्सल्य से भजा नन्द-यशोदा ने और सौहार्द्रता से भजा अर्जुन ने, सब कृतार्थ हो गये।
भाई! यही नाम की विशद महिमा है, जो अवर्णनीय और अनिर्वचनीय है।
2. राम-गीता
यह प्रसंग अरण्य काण्ड का है, गोरखपुरी-रामायण दोहा नं. 13वां से आगे -
एक बार प्रभु सुख आसीना । लछिमन बचन कहे छलहीना ।
सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई ।।
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा । सब तजि करौं चरन रज सेवा ।
कहहु ग्यान बिराग अरु माया। कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया ।।
दोहा- ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समुझाइ ।
जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ||14||
पंचवटी में एक बार भगवान राम बड़े सुख से शांत भाव से बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण ने उस सुखद, सुन्दर अवसर का लाभ उठाते हुए बड़े विनम्र भाव से उनसे पाँच प्रश्न किये।
उनके प्रश्न थे- हे प्रभु! ज्ञान क्या है? विराग क्या है? माया क्या है? भक्ति किसे कहते हैं, जिसके कारण आप भक्तों पर दया करते हैं और हे नाथ! ईश्वर और जीव में क्या भेद है? ये सब समझाकर कहिये, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह और भ्रम का निवारण हो।
इस पर भगवान राम कहने लगे-हे भाई ! मैं थोड़े में समझाकर कहता हूँ, उसे तुम मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो।
थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मति मन चित लाई ।
मैं अरु मोर तोर तै माया। जेहिंबस कीन्हें जीव निकाया ॥
मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनने का भाव मनन, चिन्तन और निदिध्यासन है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। मैं शरीर और मेरा शरीर, तू शरीर और तेरा शरीर, बस! यही माया है, जिसके वश में यद्यपि यह जीव निकाया है अर्थात बिना शरीर का है तो भी यह उसके वश में हो जाता है।
गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई ॥
गो माने इन्द्रिय, गोचर माने इन्द्रियों का विषय, जहाँ तक इन्द्रियों का विषय है, वहाँ तक माया जानो। जहाँ तक मन जाता है, चित्त चिन्तन करता है और बुद्धि निश्चय करती है वहाँ तक इन सबको, जो इन्द्रियों के विषय हैं उन्हें माया जानो।
"मैं" समरत कल्पनाओं से शून्य है। इस '' आत्मा ईश्वर में माया नहीं घटने वाली बात को भी घटित कर देती है, ऐसी यह प्रबल माया है।
बड़े-बड़े योगी, संन्यासी, विद्वान, जो संसार और माया की विवेचना कर उनकी प्राज्जियाँ उड़ा देते हैं, उन्हें भी यह माया, धन, कीर्ति, वैभव आदि में फैसा देती है।, धदों के अर्थ करने वाले, शास्त्रों की विवेचना करके उनके तत्त्व को प्रकाश देने हैं। चारले, संन्यासियों, पंडितों और विद्वानों को भी, यह बड़े चक्कर में डाल देती है। अरे! कहाँ तक कहें -
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं।
सिव बिरंचि कहुँ मोहइ । को है बपुरा आन ।।
अरी माया! तू बड़ी मोहमयी और विचित्र है, जो बात नहीं घटने वाली है उसे भी तू घटा देती है। भगवान, राम, सन्त, गुरु, महात्मा जन की असीम कृपा हो, तभी उससे पार जाया जा सकता है।
भगवान आत्मा 'मैं' में पंच महाभूतों की कल्पना जो माया कर लेती है, यद्यपि ये तीन काल में नहीं है तो भी उसमें कल्पना कर लेती है, फिर भेद डालकर जीवों को भटका रही है। वाह री माया! तू बड़ी प्रबला है।
यह माया पहिले, कल्पना करती है, पंचमहाभूतों की, फिर जीव की कल्पना करती है। फिर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर फिर स्त्री, पुरुष की, फिर वर्ण, आश्रम आदि की कल्पना कर लेती है, फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कल्पना करती है, फिर उनमें भेद डालती है और इसी भेदभाव में संसार पिसता रहता है। ये सब माया के कार्य हैं। माया की महिमा है। इसका खेल 'मैं' आत्मा आधार पर ही होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ भगवान आत्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं, वे इस माया से तर जाते हैं। अब विचार जगत् में आओ। ब्रह्म और माया, यदि ये दोनों अलग होते, भिन्न-भिन्न होते तो फिर ब्रह्म दर्शन से माया से तरना कैसे होता? इससे निश्चय होता है, प्रमाण मिलता है कि माया जो है वह भगवान आत्मा से भिन्न नहीं है, जिस तरह रज्जू और सर्प भिन्न-भिन्न नहीं है, एक ही है। अतः, रज्जू के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार भगवान और भगवान की माया ये दोनों भिन्न-भिन्न नहीं है एक ही है। इसलिए, ही भगवान के ज्ञान से माया की निवृत्ति हो जाती है।
भगवान और माया का वाच्य, वाचक संबंध है। रज्जू और सर्प, लकड़ी और डण्डा, इनका वाच्य, वाचक का सम्बन्ध है, जैसे आभूषण वाच्य है, स्वर्ण वाचक है। वस्त्र वाचक है, धागा वाच्य है। घट वाच्य है, मिट्टी वाचक है। इसी तरह स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जगत् प्रपंच, वाच्य है और 'मैं' आत्मा इसका वाचक हूँ। रज्जू और सर्प यदि भिन्न-भिन्न होते तो रज्जू के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं होती, रज्जू के जानने पर सर्प का अत्यन्ता भाव हो जाना ही सिद्ध करता है कि वे दोनों एक ही हैं। रज्जू ही अन्धकारवश सर्प दिखता है, उधर रज्जू का ज्ञान हुआ, इधर सर्प का अभाव हुआ। अज्ञान अंधकार के कारण मुझ आत्मा रज्जू में संसार प्रपंच, सर्प भासता है, अन्धकार का नाश, रज्जू का ज्ञान और सर्प का अभाव, तीनों एक ही साथ होता है आगे-पीछे नहीं। रज्जू के अज्ञान काल में भी, सर्प नहीं था, ज्ञान काल में भी सर्प नहीं, किसी काल में सर्प नहीं यह तो रस्सी ही है। इसी तरह माया, प्रपंच या संसार तीनों काल में नहीं है, वह तो 'मैं' ही हूँ।
मन माया प्रकृति जगत, चार नाम इक रूप ।
तब लग यह साँचो लगे, नहि जाना निज रूप ।।
जो माना जाय, उसका नाम है, माया। अब माया को उलट दो, हो गया 'यामा'। 'या' माने जो, 'मा' माने नहीं, अर्थात् जो नहीं हो उसका नाम है माया।
रज्जू में सर्प है क्या? सीप में चांदी है क्या? ठूंठ में पिशाच है क्या? मृगजल में जल है क्या? उत्तर है-नहीं। इसी प्रकार मुझ चैतन्य भगवान आत्मा में जगत् प्रपंच नहीं है।
भगवान का नाम है 'माया पति'। माया का पति। पति का अर्थ है स्वामी, रक्षक, आधार। डण्डे का आधार, रक्षक पति लकड़ी है। डण्डे में से लकड़ी निकाल लो, तो डण्डा रहेगा किसमें? डण्डा किसको कहोगे? डण्डे का अस्तित्व ही खतम। जैसे, लकड़ी को ही माना गया डण्डा, ऐसे ही 'मैं' आत्मा को ही माना गया माया, जब तक मैं अपने आपको कुछ मान रहा हूँ, तब तक माया मेरा पति है और ज्यों ही त्याग दिया 'मैं' को 'मैं' ही जाना तो, 'मैं' हो गया माया का पति अर्थात् 'मायापति'।
प्रश्न है- मानना किसका धर्म है?
उत्तर है-जीव का। जीव अपने आपको कुछ मानता है, मानना धर्म जीव का है। प्रश्न है-किसको मानता है? अपने आप 'मैं' को। अपने आप 'मैं' को जीव मानते ही वह परमात्मा 'मैं' से अलग हो गया, अब माया उसका पति हो गया। जब सर्व मान्यताओं का अभाव हो जाता है तब 'मैं' शुद्ध आत्मा, भगवान रह जाता हूँ, तब 'मैं' माया का पति हो गया।
मान्यता जगत् में ज्ञान नहीं और ज्ञान जगत् में मान्यता नहीं। मानने से जीव और जानने से वही भगवान है। जीव माना जाता है, भगवान जाना जाता है। मानता जीव है और जानता 'मैं' आत्मा भगवान है। यद्यपि 'मैं' आत्मा मान्यताओं से रहित हूँ तो भी मान्यता धारण कर भेद रूप दिखता हूँ। आत्मा में माया ने तीन भेद डाल दिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, फिर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहारा माया को धन्य है जो शंकर और राम में भी भेद डाल देती है। अरे यार! माया का काम ही है कि एक में दो कर देना। भेद डाल देना।यह (माया) जीव, ईश्वर, पिता-पुत्र, पति- पत्नी, राजा-प्रजा, सेवक-स्वामी, गुरु-शिष्य, भक्त-भगवान आदि कहाँ भेद नहीं डाल देती, सेवक, स्वामी, गुरु-शिष्य, भक्त-भगवान में भी इसने युद्ध करा दिया है। राम और हनुमान का, अर्जुन और कृष्ण का युद्ध हुआ है। गुरु-शिष्य का युद्ध हुआ है, सेवक-स्वामी का युद्ध हुआ है। शास्त्र और इतिहास इसके साक्षी हैं।
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ ।।
माये के दो भेद हैं- 1. विद्या माया, 2. अविद्या माया।
जो सर्वकाल में विद्यमान रहे वह विद्या और तीनों काल में जो नहीं हो, वह अविद्या माया है। 'मैं' आत्मा यह विद्या माया है और 'मैं' शरीर या मेरा शरीर, यह अविद्या माया है।
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भवकूपा ।
एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके ।
अविद्या माया दुःख रूप और दुष्ट है, जिसके वश में होकर जीव क्लेश पाते रहता है। क्षर-अक्षर, परा-अपरा, विद्या-अविद्या, अधिभूत अधिदैव और कबीर के शब्दों में जड़-चेतन ये सब एक ही भाव के शब्द हैं।
जो जगत् की रचना करे वह विद्या माया और जिसमें फँसकर जगत् का पालन करे, वह अविद्या माया है।
भगवान आत्मा राम है, लक्ष्मण जीव है, पंच भूतात्मक शरीर पंचवटी है, देहाभिमान रावण है, शांति सीता है।
ग्यान मान जहँ एकउ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ।
कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सन सिद्धि तीनि गुन त्यागी ।।
जहाँ एक का भी मान न हो (मान अर्थात् मान्यता) वह है ज्ञान।
मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ, चेतन हूँ, अच्युत हूँ, व्यापक हूँ, अद्वैत हूँ, एक हूँ, ऐसा कहना भी मान्यता ही है, जहाँ इन एक का भी मान न हो, वह ज्ञान है। 'मैं' और हूँ के बीच में जो भी शब्द हैं, अद्वैत, अच्युत, व्यापक आदि ये सब मुझसे अलग कुछ हैं, जिसे 'मैं' पर आरोपित करके कहा जा रहा है कि 'मैं' वह हूँ, तब 'मैं' और वह शब्द जो 'मैं' के बाद आया है, इस तरह द्वैत की झलक, यहाँ तक भासता है, अतः केवल शुद्ध चैतन्य धनभूत 'मैं' के अतिरिक्त, अन्य कुछ भी मान्यता जहाँ न हो वह ज्ञान है, जो केवल सत्ता मात्र है। यह एक अपेक्षा रहित है।
'अस्तित्व तत्त्व के बोध में, अस्तित्व (पदार्थ) का अभाव है।" लकड़ी के बोध में डण्डे का अभाव है, डण्डा यदि यह कहे कि मैं लकड़ी हूँ तो अभी वह ज्ञान को मानकर कह रहा है, यदि वह लकड़ी को जानकर कहना चाहेगा कि मैं लकडी हूँ, तब जब वह केवल लकड़ी है, तब किसको वह 'मैं' कहने के लिए अलग करेगा? अरे! उसे लकड़ी की अभिन्नता में यह कहते भी तो नहीं बन सकता कि मैं लकड़ी हूँ। अतः, डण्डा जब लकड़ी को जान लेगा तब वह डण्डा और लकड़ी दोनों से परे हो जायेगा।
इसी तरह 'मैं' ब्रह्म हूँ यह कहना भी मानकर कहना होगा, जान लेने पर तो 'मैं' और ब्रह्म की सत्ता एक ही है, तब कहते कैसे बनेगा कि 'मैं' ब्रह्म हूँ, क्योंकि भगवान भी अपने को भगवान नहीं कहता।
अत्यन्त वैराग्य ही निर्विकल्प समाधि के सिद्ध करने के लिए परम साधन है, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, विमल वैराग्य, इनकी व्याख्या राम-दर्शन के दूसरे भाग में लक्ष्मण-गीता के अन्तर्गत किया जा चुका है।
मन के अस्तित्व का ही त्याग यह वैराग्य है और मन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करना यह अभ्यास है।
'मन है' तब, मन, मन है, या मन 'है' है?
उत्तर है- मन 'है' है, तब 'है' अस्तित्व ही तो है, जो मन है, बस! अब मन का अस्तित्व ही गया, मन न रहा, इसी का नाम वैराग्य है।
एक शरीर में स्थित जो मान्यता है, वह मन है और सर्व शरीरों में जो मान्यता है, वह माया है। एक शरीर में स्थित जो 'मैं' है, वह आत्मा है और सर्व शरीरों में स्थित जो 'मैं' आत्मा है, वह परमात्मा है। समस्त साधनों का आधार मान्यता है, बोध नहीं।
ज्ञान की सात भूमिकाएँ हैं, ये भूमिकाएँ चित्त की होती हैं, आत्मा की नहीं। शुभेच्छा, विचारना, तन्मान्सा, तीन भूमिका तक चित्त में अज्ञान रहता है। सत्वापत्ती चौथी भूमिका में चित्त को ज्ञान होता है। पाँचवीं भूमिका में चित्त जीवन मुक्त कहलाता है, छठवीं भूमिका में चित्त बेहोश होने लगता है और सातवीं भूमिका 'तुर्यगा' में चित्त बिल्कुल बेहोश हो जाता है, इस भूमिका का योगी स्वयं क्रिया करने में असमर्थ हो जाता है। वह दूसरों के कराने से क्रिया करता है।
कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ।।
गुण तीन हैं- सत्, रज, तम।
1. सत् (सतोगुण) की सिद्धि, ज्ञान 'मैं ब्रह्म हूँ', यह ज्ञानी कहलाता है।
2. रज (रजोगुण) की सिद्धि-उपासना, 'मैं जीव हूँ' यह उपासक कहलाता है।
3. तम (तमोगुण) की सिद्धि, 'कर्म' मैं देह हूँ, यह कर्मकाण्डी कहलाता है।
भगवान राम कहते हैं कि हे तात! उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो।
दोहा- माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव ।
बन्ध मोच्छ प्रद सर्बपर माया प्रेरक सीव ।।5।।
आपु कहँ, माया ईश न जान, सो जीव कहिय। यह हुआ इस दोहे का अन्वय, इसका अर्थ है जो अपने को माया का ईश अर्थात् माया पति नहीं जानता वह जीव है और वही अपने 'मैं' को जान लिया, तब वह 'मैं' आत्मा ही है, फिर तो वह माया का ईश हो गया अर्थात् कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा 'मैं'।
जीव और ईश्वर का जो भेद है, यह भेद माना हुआ भेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है।
मुधा भेद जद्यपि कृत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ।।
(उ.का. दो. 78 के ऊपर)
श्री मानसकार कहते हैं कि यद्यपि यह भेद मुधा मिथ्या है, माया का किया हुआ है असत्य है तथापि वह बिना भगवान की कृपा के करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जाता।
'मैं जीव हूँ' 'जीव' ऐसा कहता है कि 'मैं' ऐसा कहता हूँ? उत्तर है- 'मैं' ऐसा कहता हूँ।
जीव के साथ 'है' क्रिया आती है और 'मैं' के साथ 'हूँ' क्रिया आती है, यदि हूँ क्रिया जीव की है तब तो 'मैं' जीव हूँ और यदि 'हूँ' क्रिया "मैं" की है तो फिर 'मैं' जीव नहीं हूँ, ऐसा जो नहीं जानता वही जीव है और ऐसा जो जानता है, वही 'शिव' अर्थात् 'मैं' आत्मा हूँ।
माया का अर्थ है मान्यता। 'मैं' पर ही अनन्त मान्यताएँ की गयी, तब इन अनन्त मान्यताओं का आधार (ईश) मैं ही तो हुआ, यदि 'मैं' आत्मा न होऊँ, तोये मान्यताएँ किस पर की जायेगी? 'मैं' जीव हूँ, यह 'मैं' ही मानता हूँ, अतः मान्यता 'मैं' हूँ नहीं, मान्यता से परे 'मैं' माया ईश हूँ, माया का आधार हूँ।
जीव का जीवत्व मुझ से है या जीव से है।
उत्तर है-मुझ आत्मा से है, तब बिना 'मैं' आत्मा के जीव जिन्दा नहीं रह सकता, प्रमाण लो -
दोहा- प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम ।
तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हहिं, तिन्हहिं बिधि वाम ।।290।।
चित्रकूट के जनक दरबार में, गुरु वशिष्ठ ने ऐसा कहा था। जीव और ईश्वर में भेद- 'ईश्वर' भेदरूप है या अभेद रूप? प्रश्न होता है कि भेद दो में होता है या एक में?
उत्तर है-दो में। तब यदि ईश्वर दो होकर रहेगा तो वह सीमित होगा, असीमित न होगा, पूर्ण न होगा, व्यापक न होगा, नित्य न होगा, सर्वदेशीय न होगा, अविनाशी न होगा, क्योंकि जो दो होकर रहता है वह परिछिन्न होता है, अनित्य होता है, नाशवान होता है। अतः, वह ईश्वर नहीं। यदि अभेद रूप है तो उसका किसी से भेद नहीं। अरे, जीव से क्या एक तृण से भी भेद नहीं, इस तरह सारा चराचर भगवान आत्मा 'मैं' ही है। ऐसा जो नहीं जानता, वह है जीव।
परबस जीव स्वबस भगवन्ता । जीव अनेक एक श्रीकन्ता ॥
जब तक वह परवश है तभी तक जीव है और जहाँ स्ववश हुआ कि फिर वह भगवान ही है। देखो-इस पेण्डाल में यहाँ पर इस लम्बी रस्सी के बाँध देने पर इसी एक जगह के दो नाम हो गये इस पार और उस पार। इस पार पुरुष समाज बैठा है, उस पार स्त्री समाज। अब इस रस्सी को खोल दो, निकाल दो, फिर न इस पार रहा, न उस पार। अरे! जगह तो एक ही है, वस्तुतः इसमें न इस पार है, न उस पारा इस पार और उस पार तो रस्सीकृत भेद हुआ, न कि वास्तविक। इसी तरह मुझ आत्मा रस्सी के आ जाने से, इसी एक के दो इस मन रूपी आड़ को निकाल दो, अलग कर दो, फिर न जीव रहा, न ईश्वर देवस
मैं सत्ता रूप भूमि ही अवशेष रह गया। ऐसा जो नहीं जानता, वह है जीव। 'मैं' अपने को जीव मानता हूँ, इस मान्यता का नाम है माया, मानने वाला है माया ईश और मानने पर वह हो जाता है जीव।
माया, ईश और जीव, यदि 'मैं' आत्मा न होऊँ, तो इन तीनों का आधार कौन होगा? इनका विकल्प किस पर जायेगा? इस प्रकार जो नहीं जानता वह है जीव।
जिस पर जो रहे वही उसका प्रेरक, वही उसका शासक, वही उसका आधार, और वही उसका कारण होता है। भगवान आत्मा 'मैं' पर ही तो सारा चराचर आधारित है, तब 'मैं' आत्मा ही सर्व का शासक, आधार, कारण और प्रेरक हूँ, ऐसा जो नहीं जानता, वह है जीव।
ईश्वर के जानने पर जीव नहीं, क्योंकि -
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ।।
ईश्वर को जानते ही जीव न रहा वही हो गया और ईश्वर को मानने में ईश्वर नहीं, यदि ईश्वर को मानोगे तो मान्यता विकल्प है, सत्ताहीन है, ईश्वर को मानने वाला और जानने वाला दोनों एक ही है, परन्तु वह न जीव है, न ईश्वर है। प्रश्न होता है-कि जब मानता है तब जीव होता है, तब मानने के पहिले वह क्या है?
मानने वाला न जीव है, न ईश्वर है वह अपना आप, भगवान आत्मा ही है, ऐसा जो नहीं जानता उसको जीव कहते हैं।
मंदिर में स्थापित करने के लिए, हजारों रुपये खर्च करके भगवान की मूर्ति लायी जाती है, अब यदि उस मूर्ति का कोई अंग टूट जाता है, मान लो एक उंगली ही टूट गयी, तो मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती, हजारों रुपयों में खरीदी गयी वह मूर्ति किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दी जाती है और तुरन्त दूसरी मूर्ति खरीदकर लायी जाती है और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर उसे मंदिर में स्थापित की जाती है।
भैय्या! इसका रहस्य समझो-हम जिस ब्रह्म के उपासक हैं वह पूर्ण है, अखण्ड है, अतः खण्डित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। एक तृण को भी यदि भगवान से भिन्न माना, भगवान से अलग किया कि भगवान खण्डित हो गया, अखण्ड न रहा, इसलिए सर्व भगवान है, उससे किसी का भेद नहीं।
जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पशक्ति वाला है, ईश्वर सर्व शक्तिमान है, जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। इस तरह जीव और ईश्वर को, बुद्धिरूपी तराजू के अलग-अलग पलड़े में रखकर कौन तौल रहा है, तौलने वाला कौन है? यदि वह जीव है, तब तो वह पलड़े में रहेगा, तब तौलेगा कौन? बस, यह जो तौल रहा है, वही 'मैं' आत्मा है, जो जीव और ईश्वर दोनों का ज्ञाता, दोनों से परे है।
जीववादी जीव को ईश्वर का अंश कहते हैं-पत्थर का अंश पत्थर, मिट्टी का अंश मिट्टी, लोहे का अंश लोहा और सोने का अंश सोना है, अंश का अर्थ है खण्ड, टुकड़ा।
पत्थर का अंश मिट्टी नहीं होता, लोहे का अंश पत्थर नहीं होता और सोने का अंश लोहा नहीं हो सकता, इसी तरह ईश्वर का अंश ईश्वर ही होगा, जीव नहीं हो सकता।
प्रश्न होता है, तब मानसकार ने ईश्वर अंश जीव क्यों लिखा ? इसका उत्तर आगे इसी पुस्तक में मिलेगा।
यदि भगवान को हम परमपिता कहें, हम सब उनकी संतान हैं, तब जिस तरह ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र होता है, क्योंकि जो जाति पिता की, वही जाति पुत्र की होती है। इसी तरह जब हम ईश्वर की सन्तान हैं, पुत्र हैं, तब हम ईश्वर ही हैं, जीव कैसे? जीव जाति हमारी नहीं हो सकती। पिता, पुत्र की एक ही जाति होगी।
जीव साकार ईश्वरका अंश है या निराकार ईश्वर का? देखो यह फूल साकार है, इसमें से इसका अंश निकालते जाओ, इसका खण्ड करते चले जाओ, तब अंत में खण्ड होते-होते, अंश निकालते-निकालते इस फूल का अंत हो जायेगा। इसी तरह यदि जीव को साकार ईश्वर का अंश कहो तो उस साकार ईश्वर का भी अंत हो जायेगा, वह ईश्वर ही समाप्त हो जायेगा, इससे सिद्ध हुआ कि जीव, साकार ईश्वर का अंश नहीं है। अब यदि जीव को निराकार ईश्वर का अंश कहो तो देखो इस फूल में सुगन्ध निराकार है, उसका अंश हो सकेगा ? उसका खण्ड कैसे करोगे, ऐसे ही यह आकाश निराकार है, तब आकाश का खण्ड अथवा अंश नहीं किया जा सकता, इस तरह जीव निराकार ईश्वर का भी अंश सिद्ध नहीं होता।
जीव छोटा-बड़ा नहीं होता, यदि वह छोटा-बडा होगा तब चींटी में जो जीव है, वह छोटा और हाथी में जो जीव है, वह बड़ा होगा, इस स्थिति में हाथी का जीव अपना कर्मफल भोगने के लिए जब चींटी के शरीर में प्रवेश करेगा, तब चींटी के छोटे शरीर में हाथी का बड़ा जीव जितने अंश तक समा सकेगा, उतना समाएगा और शेष जीव चींटी के शरीर के बाहर खिचड़ता फिरेगा, इस तरह इस जीव की बड़ी दुर्गति होगी, ऐसे ही चींटी में का जीव जब अपना कर्मफल भोगने हाथी के शरीर में जायेगा तब चींटी का वह छोटा जीव हाथी के उस बड़े शरीर में थोड़ी जगह में ही समा जायेगा, तब हाथी के शरीर का शेष भाग जीव से शून्य होगा। इस निश्चय से यह सिद्ध होता है कि जीव छोटा-बड़ा नहीं होता।
प्रश्न होता है कि ईश्वर इदंगम्य है या अहंगम्य है। यदि वह इदंगम्य है तो दो हो गया फिर वह पूर्ण न रहा और यदि अहंगम्य है तो मुझ से भिन्न नहीं 'मैं' ही हूँ। जिस तरह आकाश घट (घड़ा) और मठ (मकान), घट और मठ के बाहर एक ही है, परन्तु घट में रहने से उसका नाम घटाकाश, मठ में होने से उसी का नाम मठाकाश और घट और मठ दोनों के बाहर, उसी आकाश का नाम वृहदाकाश हो जाता है। यद्यपि, घटाकाश, मठाकाश और वृहदाकाश ये तीनों आकाश नहीं हैं, अरे यार! आकाश तो एक ही है, जो घट, मठ और इनके बाहर है, परन्तु घट में होने से उसी आकाश का घट उपाधि के कारण घटाकाश और मठ में होने से उसी आकाश का मठ उपाधि के कारण मठाकाश नाम पड़ गया और इन दोनों के बाहर वह निरुपाधि शुद्ध, पूर्ण आकाश ही है, जो निर्विकार है, सर्व उपाधियों से रहित है। इसी तरह माया उपाधि से, मुझ चैतन्य घनभूत, आत्मा का नाम हुआ ईश्वर, अविद्या उपाधि से उसी का नाम जीव और दोनों उपाधियों से रहित, जो शुद्ध चेतन है, वह है ब्रह्म।
अपने आप 'मैं' आत्मा को न जानना अविद्या है इस अविद्या उपाधि के कारण जीव। अपने आप 'मैं' आत्मा को कुछ मानना यह है माया इस उपाधि से ईश्वर। इन दोनों उपाधि से रहित जो है वह है ब्रह्म।
प्रश्न होता है-अज्ञान 'मैं' हूँ या मुझमें अज्ञान है?
यह उत्तर है- अज्ञान मैं हूँ, न अज्ञान मुझमें है, इस ज्ञान के अज्ञान को ही अविद्या कहते हैं, इस उपाधि के कारण ही जीवा 'मैं' माया हूँ या मुझमें माना गया है?
उत्तर है- मुझ पर मान्यता है। अतः 'मैं' मान्यता से परे हो गया, इस उपाधि से रहित, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ।
धर्म ते बिरति जोग ते ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ।।
जातें बेगि द्रवउँ मैं भाई । सो सम भगति भगत सुखदाई ॥
धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है ऐसा वेदों में वर्णन किया है और भाई! जिससे में शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ यह मेरी भक्ति जो भक्तों को सुख देने वाली है।
सो सुतंत्र, अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ।
वह भक्ति स्वतंत्र है, जिसके अधीन ज्ञान और विज्ञान है। अहं ब्रह्मरिम 'मैं' ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान है। 'अहमेवेदं सर्वं' 'मैं' सर्व हूँ, यह विज्ञान है और 'मैं' हूँ, यह भक्ति है। 'मैं' ब्रह्म हूँ यह ज्ञान और 'मैं' सर्व हूँ, यह विज्ञान इन दोनों में से 'मैं' को निकाल लो तो वे व्यर्थ हो गये, दोनों न रहे। इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों की सिद्धि 'मैं' के बिना नहीं है। अतः, ज्ञान और विज्ञान दोनों 'मैं' हूँ, इस भक्ति के अधीन हुए। यह भक्ति परम स्वतंत्र है।
भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो सन्त होईं अनुकूला ॥
ऐसी यह भक्ति अनुपम है, जिसकी उपमा विश्व में नहीं, फिर वह सर्व सुखों की जड़ है, ज्ञान-विज्ञान तो साधन जन्य हैं, परन्तु 'मैं' हूँ यह भक्ति जो है, उसके लिए कोई साधन नहीं है, यह तो केवल कृपा जन्य है, यह गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। जब सन्त मिल जायँ और वे अनुकूल हो जायँ, तभी उन संतों की कृपा से ही वह भक्ति मिलती है। जिन सन्तों की कृपा से ऐसी भक्ति प्राप्त होती है वे सन्त, जब भगवान की कृपा होती है, तभी मिलते हैं। मतलब यह कि भगवान की कृपा से सन्त मिलते हैं और सन्त की कृपा से भगवान मिलते हैं। इन सन्तों में और भगवान में भेद का अभाव है अर्थात् वे दोनों एक ही हैं। अतः, भगवान की प्राप्ति के लिए साधन मत करो, सन्तों की प्राप्ति का ही साधन करो, जितने साधन हैं वे हमारे हृदय को भगवत स्वरूप संतों की प्राप्ति का पात्र बनाते हैं।
भगति कि साधन कहउँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ।
प्रथमहिं बिप्र चरन अति प्रीती। निज-निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥
एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा ।
श्रवनादिक नवभक्ति दृढ़ाहीं । ममलीला रति अति मन माहीं ॥
सन्त चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ।
गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा । सब मोहि कहें जाने दृढ़ सेवा ॥
मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ।
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस मैं ताकें ॥
दोहा- बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम ।
तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउ सदा विश्राम ।।16।।
भक्ति जो है, वह अनिर्वचनीय है, मन वाणी से परे है वह बखानी नहीं जा काकती। भक्ति के साधन का बखान है, भक्ति का बखान नहीं है, मानसकार साफ तो कह रहे हैं कि भक्ति के साधन कहीं बखानी, न कि "भक्ति बखानी"।
भक्ति दो प्रकार की होती है - 1. अपरा भक्ति, 2. पराभक्ति ।
1. अपरा भक्ति - सगुण भगवान की भक्ति, इसमें भक्त और भगवान का भेद रहता है, इसका आधार है 'भावना'।
भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान गुरु (भगवान सब में लगा रहेगा) की मूर्ति की भावना की जाती है और उसे हृदय मंदिर में स्थापित कर फिर उस मूर्ति की आराधना की जाती है, इस भावना का फल है प्रेम और प्रेम का फूल है भक्त भगवान की एकता। इस एकता का फल है चित्त की परम शांति। यह अपरा भक्ति है।
2. परा भक्ति - यह निर्गुण उपासना है, यह अभेद उपासना है। इसका आधार है विचारा विचार का फल है ज्ञान। ज्ञान का फल है-जीवात्मा, परमात्मा की एकता। इस एकता का फल चित्त की परम शांति। किष्किन्धा काण्ड का एक दोहा है -
दोहा- चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि ।
जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ||16|1
(कि.का.दो.-16)
वर्षा ऋतु के बीत जाने पर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी, जो वर्षा के कारण नगर में रुके रहते हैं। शरद ऋतु पाकर उस नगर को त्यागकर वे क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए अन्यत्र चले जाते हैं, जैसे 'हरि भक्ति' को पाकर मनुष्य चारों वर्ण और आश्रम का त्याग कर देते हैं।
वर्ण धर्म-मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूँ।
आश्रम धर्म - मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यासी हैं। ये ही वर्ण और आश्रम के अभिमान हैं। 'हरि भक्ति' प्राप्त हो जाने पर इनके अभिमान का त्याग हो जाता है, ये अभिमान त्याग दिये जाते हैं।
वर्णाश्रमाभिमान, देहाभिमान पर अवलम्बित है और देहाभिमान, देहाध्यास पर आधारित है तथा देहाध्यास, स्व-स्वरूप भगवान आत्मा 'मैं' के अज्ञान पर आधारित है। इसका स्वरूप समझो, जो चीज जैसी हो उसको वैसी न जानकर, उसको कुछ का कुछ मान लेना यही अध्यास है, जैसे- रज्जू के अज्ञान से, रज्जू में ही सर्प का अध्यास है, इसी प्रकार स्व-स्वरूप भगवान आत्मा के अज्ञान से उसमें ही देह का अध्यास होता है।
देह के अध्यास के बाद फिर मैं देह हूँ यह देह का अभिमान आया, फिर स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बालक, युवा, वृद्ध हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूँ। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यासी हूँ आदि। वर्ण और आश्रम का अभिमान आया। जब भगवान आत्मा 'मैं' का बोध हुआ तब भगवान आत्मा 'मैं' को ही जो माना था उसका अभाव हो गया, उसका अपने आप त्याग हो गया।
जिमि हरि भगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ।।
हरि भक्ति कहो, हरि पद कहो अथवा भक्ति कहो सबका एक ही भाव है। जितनी मान्यताएँ थीं देहादिक का, उन सबका त्याग हो गया।
पहिले अध्यास का त्याग होता है, फिर अभिमान का त्याग होता है, इसके बाद वर्णाश्रमाभिमान का त्याग होता है, यही वर्ण और आश्रम का त्याग है।
सेवक, सेब्य भाव बिनु, भव न तरिअ उरगारि ।।
इसका स्पष्ट अन्वय है, हे उरगारि!
सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिय ।।
अर्थात् सेवा करते-करते जब तक सेवक में सेव्य भाव न आ जाय, तब तक है उरगारि! वह भव से नहीं तर सकता, इसका अर्थ है, सेवक सेव्य की एकता, दोनो का एक हो जाना ।।
श्याम-श्याम रटते-रटते, राधा श्याम भई ।
तब राधा पूछत सखियन सों राधा कहाँ गई ?
अरे! गयी कहाँ? स्वयं श्याम हो गयी, फिर राधा कहाँ मिलेगी। उसका अस्तित्व ही खतम। नदी, समुद्र में मिलते ही समुद्र हो गयी, फिर ढूँढ़ने पर समुद्र में नही मिलने वाली नहीं है। यह है परा भक्ति।
एक भक्ति और है, जो न परा है, न अपरा है। न भेद है, न अभेद है। वह 'मैं' पद है। यह न सगुण है, न निर्गुण है, जो कागभुशुण्डी को मिली थी।
दोहा- अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव ।
जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ।।
(उ.कां. 84-क)
वह भक्ति कैसी है?
परम प्रकास रूप दिन राती । नहिं कछु चहिअ दिआ घृत बाती ।।
भक्ति की उपमा, चिन्तामणि से दी गयी है। भक्ति चिन्तामणि को तुम जिस दृष्टि से देखना चाहो उसी रूप में वह दिखती है।
कर्म काण्डी को 'मैं' देह हूँ। 'मैं' आत्मा, देह रूप में दिखता है।
उपासक को 'मैं' जीव हूँ। 'मैं' आत्मा, जीव रूप में दिखता हूँ।
ज्ञानी को 'मैं' ब्रह्म हूँ। 'मैं' आत्मा, ब्रह्म रूप में दिखता हूँ।
नास्तिक को 'मैं' आत्मा, 'नहीं है' रूप में दिखता हूँ और आस्तिक को 'मैं' आत्मा 'है 'इस रूप में दिखता हूँ। इस तरह जो जिस भाव में देखता है, उसे उसी रूप में दिखता हूँ।
बिना बोध के न सगुण रूप में निष्ठा हो सकती है और न निर्गुण रूप में ही। भैय्या! इन रूपों में तथा चरित्र और लीला में रत तो ज्ञान के बाद ही होता है, अज्ञानी क्या जानेगा कि क्या सगुण और क्या निर्गुण है।
देखकर जाना जाता है और सुनकर माना जाता है। अपने स्वरूप 'मैं' आत्मा को जब देख लेता है, तभी उसमें प्रीति होती है।
जानें बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होई नहिं प्रीती ।
प्रीति बिना नहिं भगति दिढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई ।।
(उ.कां.)
सगुन को भगवान शंकर के समान भजना चाहिए, लीला और चरित्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आधार पर ही स्थित रहना चाहिए।
माता पार्वती और गरुड आदि लीला और चरित्र के चक्कर में पड़ गये, इसलिए ही उन्हें बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। परम वैराग्यवान को चाहिए कि वह लीला और चरित्र के चक्कर में न पड़े, वे भगवान शंकर की दृष्टि को अपनायें।
भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥
भगवान राम के श्री मुख द्वारा इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी बड़े सुखी हुए और उन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में सिर नवाया।
बस! यहीं पर राम गीता का उपसंहार है।
जर्रा- जर्रा भगवान है, कण-कण भगवान है, परन्तु इसका आनन्द तो तभी आयेगा, जब तुम अमली जामा पहिनोगे, इसके बिना यह आनन्द दूर ही है। अपने को इस ढाँचे में ढालो।
3. विभीषण शरणागति
आज का प्रसंग है सुन्दर काण्ड के अन्तर्गत विभीषण -
शरणागति, गोरखपुरी रामायण दोहा नं. 37वाँ -
दोहा- सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस ।
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगहीं नास ।।
(सु.कां.दो.-37)
मंत्री, बैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय से या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। मंत्री यदि इस भय से कि राजा को मेरी नेक सलाह अप्रिय लगेगी, जिससे वे अप्रसन्न होकर मुझे मंत्री पद से अलग कर देंगे, ठकुर सुहाती बोलता है और राजा को गलत मार्ग से नहीं रोकता तो उस राजा का और उस राज्य का विनाश अवश्य ही शीघ्र हो जायेगा। ऐसे ही वैद्य रोगी की अप्रन्नता के भय से, रोगी के कुपथ मांगने पर (एक सौ चार डिग्री बुखार चढ़ा है और रोगी खाने को दही मांग रहा है) उसे दे देता है तो उस रोगी के शरीर का विनाश ही समझो, वह जीवित नहीं रह सकता। ऐसे ही यदि शिष्य की अप्रन्नता के भय से गुरु उसे गलत रास्ते से नहीं रोकता, कुमार्ग पर जाने देता है तो गुरु और शिष्य दोनों के धर्मों का नाश हो जाता है।
सोइ रावन कहुँ बनी सहाई । अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई ।
अवसर जानि विभीषनु आवा । भ्राता चरन सीसु तेहि नावा ॥
रावण के लिए भी वही संयोग उपस्थित है, मंत्री उसे सुना-सुनाकर गलत मार्ग पर जाते देखकर भी, उसके मुँह पर उसकी प्रशंसा किये जा रहे हैं। ठीक समय, अवसर जानकर विभीषण आये और उन्होंने बड़े भाई (रावण) के चरणों में सिर नवाया।
पुनि सिरु नाइ बैठि निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ।
जौ कृपाल पूँछिहु मोहि बाता । मति अनुरूप कहउँ हित ताता ।।
फिर वे अपने आसन पर बैठ गये और आज्ञा पाकर कहने लगे कि हे कृपालु ! जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात! मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ।
जो आपन चाहै कल्याना। सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना।
सो पर नारि लिलार गोसाई। तजउ चउथि के चन्द की नाई ।।
जो कोई भी यदि अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, तो हे स्वामी! वह पराई स्त्री के ललाट को चौथ की चन्द्रमा की तरह त्याग दे। जैसे लोग चौथ के चन्द्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री के मुख को न देखें।
षट् ऋतु, बारह मास है, तामें शिशिर बसन्त ।
तामें वह दिन कौन है, सती तजत है कन्त ॥
वह चतुर्थी माघ महीने का है, जिस दिन माता सती भगवान शंकर के मुख को नहीं देखती, क्योंकि भगवान शंकर के मस्तक में चन्द्रमा लगा था जिसका लम्बा इतिहास है।
चौदह भुवन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्टइ नहिं सोई ।
गुन सागर नागर नर जोऊ । अलप लोभ भल कहइ न कोऊ ॥
चौदह भुवनों का एक ही मालिक हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और बड़ा ही चतुर क्यों न हो, यदि उसमें थोड़ा भी लोभ दिखता है तो उसे कोई भला नहीं कह सकता।
काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पन्थ ।
सब परिहरि रघुबीरहिं, भजहु भजहिं जेहि सन्त ||38||
जिसे नरक न जाना हो वह काम, क्रोध, मद और लोभ, इन विकारों से सदा बचता रहे, वह इन तीनों का सर्वथा त्याग कर दे, जबकि आज दुनिया में त्रिदोष हो गया है, सन्निपात हो गया है। काम विकार इतना बढ गया है कि क्या कहा जाये लोगो को अपना पराया नहीं सूझ रहा है। लोभ ऐसा बढ गया है कि बाजार में चीजों में मिलावट का साम्राज्य है, खोजने से शुद्ध जहर भी मिलना मुश्किल है, क्रोध ऐसा बढ गया है कि एक-दूसरे को पा जायें तो खा जायें, अब विश्व युद्ध की तैयारी है। अब की बार यदि विश्व युद्ध हुआ तो वह अधिक दिन नहीं चलेगा, दो-चार दिनों में ही सब समाप्त हो जाने वाला है। भाई! सरकार में तुम्हारी श्रद्धा भले न हो, पर उसके देश में रहकर उसके बनाये हुए विधान का तुम उल्लंघन कदापि नहीं कर सकते। यदि करोगे तो दण्ड के भागी होगे, सरकार तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, यह तुम्हें अवश्य सजा देगी। उसी प्रकार ईश्वर के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भले ही न हो, तुम उसे न मानो, परन्तु उसके विधान को तुम्हें मानना पड़ेगा अन्यथा प्रकृति तो तुम्हें दण्ड देगी ही, छोड़ेगी नहीं। चीजों में मिलावट करना, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, परायी बहू-बेटियों को बुरी निगाह से देखना, हिंसा करना, दूसरों का अहित चाहना आदि क्या ये सब काम ईश्वरीय विधान के प्रतिकूल नहीं है, तब तुम उस मालिक के देश में निरपराधी कैसे सिद्ध होगे, फिर तुम्हें स्वप्न में भी, सुख और शांति कहाँ मिलने वाली है। इसलिए होश में आ जाओ अन्यथा भोग तो रहे ही हो। विभीषण कहते हैं कि-
तात राम नहिं नर भूपाला । भुवनेस्वर कालहु कर काला ।
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । ब्यापक अजित अनादि अनंता ।।
हे तात! राम केवल मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं, वे सम्पूर्ण, ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भण्डार भगवान हैं, वे सर्व विकारों से रहित, अजन्मा, व्यापक, अनादि और अजेय ब्रह्म हैं।
गो द्विज घेनु देव हितकारी। कृपा सिन्धु मानुष तनुधारी ।
जन रंजन भंजन खल ब्राता। वेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता ।।
उन कृपा के समुद्र भगवान ने, पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई! वे सेवकों को आनन्द देने वाले, दुष्टों के समूह को नाश करने वाले और वेद तथा धर्म के रक्षक हैं।
देखो - भगवान के तीन रूप हैं -
1. आधिभौतिक, 2. आधिदैविक और 3. आध्यात्मिक।
यह सारा चराचर जो मन वाणी का विषय है और दृष्टि गोचर हो रहा है, वह भगवान का आधिभौतिक रूप है, इसमें अज्ञानी को संसार का भ्रम हो रहा है, वह इसे संसार मानता है, यद्यपि सन्त महात्मा जन, वेद, शास्त्र, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, चिल्ला-चिल्लाकर कह रही है कि ये सारा चराचर भगवान ही है, वासुदेव है, नारायण है-
सीय राममय सब जग जानी
जड़ चेतन, जग जीव जत सकल राम मय जानि ।।
सर्व खल्वमिदं ब्रह्म नेहनानास्ति किं चन ।।
परन्तु इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? इसे मोह कहते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये लीला विग्रह शरीर भगवान का अधिदैविक रूप है, इसमें अज्ञानी जनों को नर का भ्रम होता है, यह महा मोह है। यह भ्रम माता सती को, गरुड़ को और भुशुण्डी आदि को हुआ था।
सती को भ्रम हुआ -
जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि ।
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ।।
गरुड को भ्रम हुआ -
भव बंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम ।
खर्ब निसाचर बाँघेउ नागपास सोइ राम ।।
भुसुण्डी को भ्रम हुआ -
प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह ।
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द सन्दोह ।।
सर्व में जो 'मैं' नाम से प्रसिद्ध है और जो नित्य सब में प्रस्फुटित हो रहा है, वह भगवान का आध्यात्मिक रूप है इसमें अज्ञानी जनों को जीव का भ्रम हो रहा है, वह समझता है कि 'मैं' संसारी जीव हूँ, यह सम्मोह है।
जैसे सर्प का अत्यन्ता भाव रज्जू देश में देखने में है, सर्प देश में जो सर्प दिख रहा है वह 'है' अस्तित्व ही है और प्रपंच देश से देखने पर प्रपंच भासता है, जो अस्तित्व ही है।
यद्यपि संसार तीन काल में है ही नहीं, परन्तु जब तक भगवान आत्मा 'मैं' का बोध न हो जायेगा, तब तक इसका अनुभव कैसे होगा? और बिना अनुभव के विश्वास कैसे हो सकता है? आत्मा के ज्ञान से सर्व का ज्ञान, आत्मा के दर्शन से सर्व का दर्शन और आत्मा के अनुभव से सर्व का अनुभव होता है। इसलिए ही वेद शास्त्र, सन्त महात्माजन कहते हैं कि आत्म दर्शन करो, आत्मा को जानो, आत्मानुभव करो।
जो वास्तविक तत्त्व है, वह जाना जाता है और जहाँ तक मन, वाणी का विषय है वह माना जाता है। आत्मा उसको कहते हैं जो सर्व का आधार है, कारण है, अधिष्ठान है और सर्व का अस्तित्व है, बिना ज्ञान के मोह और भ्रम का नाश नहीं होता, इसलिए अपने 'मैं' को जानो, आत्म ज्ञान प्राप्त करो, इसके बिना सब व्यर्थ है।
चतुराई चूल्हे परै, घूरे परै अचार । तुलसी आतम ज्ञान बिनु, चारों वर्ण चमार ॥
विभीषण कहते हैं, हे भैय्या रावण! वही ब्रह्म भगवान ही ये राम हैं, यह भगवान का लीला विग्रह शरीर है। उन्हें मनुष्य और राजा मत मानो, वे अजन्मा, निर्विकार, अजेय और अनादि हैं इसलिए हे भाई!
ताहि बयरु तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ।
देहु नाथ प्रभु कहुँ बैदेही । भजहु राम बिनु हेतु सनेही ।।
बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुःख नाश करने वाले हैं, हे नाथ! उन प्रभु को, जानकी जी दे दीजिये और बिना कारण ही स्नेह करने वाले श्रीराम को भजिये ।
सरन गएँ प्रभु ताहु ना त्यागा। बिस्व द्रोह कृत अघजेहि लागा ।
जासु नाम त्रय ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रगट समुझु जियें रावन ।।
जिसे सम्पूर्ण जगत् से द्रोह करने का भी पाप लगा हो, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते, जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु (भगवान) मनुष्य रूप में प्रगट हुए हैं। हे रावण! हृदय में यह समझ लीजिये।
दोहा- बार-बार पद लागऊँविनय करउँ दससीस ।
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ।।39-क।।
हे दशशीश! मैं बार-बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्यागकर आप कौशल पति श्री रामजी का भजन कीजिये -
दोहा- मुनि पुलस्ति निज सिष्यसन कहि पठई यह बात ।
तुरत सो मैं प्रभुसन कही पाइ सुअवसरु तात ।।39 ख।।
मुनि पुलस्त्यजी ने अपने शिष्य के हाथ बात कहला भेजी है। सो, हे तात! सुन्दर अवसर पाकर मैंने तुरन्त ही यह बात आपसे कह दी।
विभीषण के इस कथन का माल्यवन्त जो कि रावन का बुद्धिमान मंत्री था उसने भी समर्थन किया और कहा कि हे तात! आपके छोटे भाई विभीषण नीतिवान है, वे जो कुछ कह रहे हैं, उन्हें हृदय में धारण कीजिये, इसी में आपका परम हित है।
विभीषण और माल्यवन्त के इन बातों को सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और कहने लगा कि ये दोनों मूर्ख, शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं अरे! यहाँ कोई है? इन्हें बाहर निकालो यहाँ से, तब माल्यवन्त तो घर चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे -
सुमति कुमति सबकें उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं ।
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना ॥
हे नाथ! पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है, जहाँ सुबुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की सुख सम्पदाएँ रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है, वहाँ परिणाम में विपत्ति का साम्राज्य रहता है।
तव उर कुमति बसी बिपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ।।
कालराति निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥
हे भाई ! आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसलिए ही आप हित को अहित और मित्र को शत्रु मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीताजी पर आपकी बड़ी प्रीति है।
दोहा - तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार ।
सीता देहु राम कहुँ, अहित न होइ तुम्हार ।।40।।
हे तात ! मैं चरण पकड़कर आपसे यही भीख माँगता हूँ कि आप मुझ छोटे भाई का दुलार रख, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिये और श्री रामजी को सीता जी दे दीजिये, जिससे आपका अहित न हो।
बुध पुरान श्रुति संमत बानी । कही बिभीषन नीति बखानी ।
सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ।
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपुकर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ।
कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता मैं नाही ।
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती। सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती।
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहिं बारा ॥
विभीषण ने रावण से पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला- रे दुष्ट! अब मृत्यु तेरे निकट आ गयी है। अरे मूर्ख! तू मेरे जियाए जीता है और शत्रु का पक्ष लेता है। मेरे नगर में रहकर उन तपस्वियों पर प्रेम करता है, अतः अरे मूर्ख! जाकर उन्हीं को यह नीति बता, ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारा, परन्तु छोटे भाई विभीषण ने लात से मारने पर भी बार-बार उनके चरण ही पकड़े।
उमा संत कइ इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥
सन्त की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों पर भलाई ही करते हैं।
भलो भलाइहि पै लहइ, लहइ निचाइहि नीचु ।
सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ मीचु ।।
भैय्या! बैरागी, सन्यासी, उदासी होना सरल है, मगर सन्त होना बड़ा कठिन है।
सर्वे सर्पे न माणिक्यं, मौक्तं न गजे-गजे ।
साधवः नहि सर्वत्र, चन्दन न बने-बने ॥
प्रत्येक सर्प में मणि नहीं होती, हर एक हाथी में गज मुक्ता नहीं होता, सन्त महात्मा जन सर्वत्र नहीं मिलते और हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते, ये तो कहीं-कहीं ही सुलभ हो सकते हैं।
संतन्ह के महिमा रघुराई। बहु बिधि वेद पुरानन्ह गाई ।।
यदि सन्त मिल गये तो जान लो, भगवान मिल गये। जैसे हजारों ठोकर खाकर एक आभूषण बनता है, उसी प्रकार हजारों लाखों मुसीबत सहकर एकसन्त होता है। 'सबहिं मानप्रद, आपु अमानी।' सन्त स्वयं अमानी होता है, परन्तु सबको वे मान दिया करते हैं। तारीफ तो यही है कि सन्तों द्वारा मिला सम्मान सबको हजम नहीं होता, हजम नहीं होने पर यह उन्माद का कारण बन जाता है।
सन्त, मन से, वचन से और कर्म से नित्य बह्मामृत में डूबे रहते हैं। वे दिन-रात जगत के जीवों के कल्याण की ही कामना करते रहते हैं। संत दूसरों में एक अणु के बराबर भी गुण देखते हैं तो उसे वे पहाड़ के समान समझते हैं, वे जिनका आदर करते हैं उसे वे भूल जाते हैं, परन्तु दूसरे यदि थोड़ा भी उपकार करते हैं, वे जीवन भर याद करते हैं।
साघु चरित सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गुनमय फलजासू ।
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बंदनीय जेहिंजग जस पावा ।।
जैसे कपास अनेक दुःखों को सहन करके भी पराये छिद्र को ढाँकता है, इसी तरह सन्त अनेक मुसीबतों को सहकर भी दूसरे का कल्याण करते हैं, इसीलिए श्री मानसकार कहते हैं कि -
बिधि हरि हर कबि कोबिद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी।
सो मो सन कहि जात न कैसें । साक बनिक मनि गुन गन जैसें ।।
भगवान को जानना बड़ा आसान है, क्योंकि भगवान अपना 'मैं' है, अपना आप है, 'स्व' रूप है, परन्तु भगवान को जानने वाले जो सन्त हैं, जो भगवान को जानते हैं, उनको पहचानना बड़ी मुश्किल है। उनके अत्यंत निकट रहकर भी, वे जाने नहीं जा सकते और यदिजान लिया तो फिर वे जीवन भर के लिए उनके हो गये।
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ।।
जिन्हें कीर्ति, कंचन की वासना रहती है, वे ही वेशभूषा धारण करते हैं और जिनकी कोई कामना ही नहीं, उन्हें भेष से क्या प्रयोजन।
ऊषर बरषइ तृन नहिं जामा। जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ॥
तो फिर वह क्या वेशभूषा बनायेगा इसलिये संतों का कोई भेष नहीं होता। तब प्रश्न होता है कि स्वामीजी ! इस स्थिति में हम उन्हें किस तरह पहिचाने? उत्तर है- भैय्या। इसकी जिम्मेदारी तुम अपने सिर पर मत लो तुम केवल अपने अंदर योग्यता पैदा करो हृदय में मछली के समान तड़प पैदा करो अपने आपको अधिकारी बनाओ, फिर तो तुम्हें वे खुद खोजते हुए, तुम्हारा नाम, गाँव का पता पूछते हुए तुम्हारे पास पहुँच आयेंगे उन्हें खोजने तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
देखो, इतने महान आत्मा, सिद्ध पुरुष जगत् के कल्याणार्थ पृथ्वी मंडल पर बिचरते रहते हैं -
इनकी ये सरकारी ड्यूटी है- है -
कुमारो नारद ऋभुरङ्गिरा देवलो ऽसितः
अपान्तरतमो व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गौतमः ।
वसिष्ठो भगवान् रामः कपिलो बादरायणिः ।
दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातूकर्ण्यस्तथाऽऽरुणिः ।।
रोमशश्च्यवनो दत्त आसुरिः सपतञ्जलिः ।
ऋषिर्वेदशिरा बोध्यो मुनिः पञ्चशिरास्तथा ।
हिरण्यनाभः कौसल्यः श्रुतदेव ऋतध्वजः ।
एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः ।।
(श्रीमद् भागवत, षष्ठंस्कन्ध, अध्याय 15 चित्रकेतु उपा., पृ. 290)
कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपान्तरम, व्यास, मार्कण्डेय, गौतम, वशिष्ठ, राम, कपिल, बादरायणि, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, अरुणि, रोमश, च्यवन, दत्तात्रय, आसुरि, पतञ्जलि, वेदशिरा, बोद्धय, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव और ऋतुध्वज।
सम्राट परीक्षित के समय तक ये प्रत्यक्ष दिखाई देते थे, परन्तु अब जैसे-जैसे लोगों की दृष्टि में दोष आता गया वैसे-वैसे ये लोग लोप होते गये, मगर विचरते हैं आज भी। जिनको देख लेते हैं कि ये अधिकारी हैं, उनको ये दर्शन देते हैं और उनका कल्याण करके चले जाते हैं। इसलिए तड़प पैदा करो तब संत मिलेगा नहीं तो लाटरी का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता।
भगवान के चार प्रकार के अवतार हैं -
1. नित्य अवतार,
2. नैमित्तक अवतार,
3. प्रादुर्भाव अवतार
4. आतुर अवतारा
भगवान राम और कृष्ण का अवतार रावण और कंस के वध करने के निमित्त हुआ था। दुष्टों का संहार और भक्तों को सुख पहुँचाने यह भगवान का नैमित्तक अवतार है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के निमित्त खम्भ फाड़कर नरसिंह अवतार हुआ यह भगवान का प्रादुर्भाव अवतार है। गजेन्द्र की रक्षा के लिए जो अवतार हुआ वह भगवान का आतुर अवतार है और नित्य अवतारों में भगवान सन्त आते हैं, जिनके द्वारा जगत् का अहर्निश कल्याण होते रहता है। जब विभीषण को रावण ने लात मारकर निकाल दिया, तब वह यह कहते हुए वहाँ से चला कि भाई! तुम पिता के तुल्य हो, मुझे यदि आपने मारा भी तो कोई हानि नहीं, परन्तु हे नाथ! मैं फिर भी कहता हूँ कि आपका भला, श्रीराम के भजने में ही है। ऐसा कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ ले आकाश मार्ग में गये और सबको सुनाकर वे कहने लगे - -
रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरि ।
मैं रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ।।41।।
भगवान आत्मा राम सत्य संकल्प हैं, उसे जानना चाहिए। भगवान राम ने, अभी-अभी ऋषियों के आश्रम में प्रतिज्ञा की थी कि-
निसिचर हीन करउँ महि। भुज उठाय पन कीन्ह ।
जिस स्थान पर यह प्रतिज्ञा हुई है, वह स्थान नागपुर जिले में आज भी "रामटेक'" (राम की प्रतिज्ञा) के नाम से प्रसिद्ध है।
विभीषण रावण से कहते हैं कि राम सत्य संकल्प है, उनका संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, असत्य नहीं होता, इसलिए हे रावण! तेरी सभा काल के वश में है, अतः अब मैं श्री रगुबीर के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना।
अस कहि चला बिभीषनु जब हीं। आयूहीन भये तब सबहीं।
साधु अवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल कै हानी।
रावन जबहिं बिभीषन त्यागा। भयउ बिभव बिनु तबहिं अभागा ।
चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ।।
ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गये, उनकी मृत्यु निश्चित हो गयी। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी! साधु का अपमान तुरन्त ही सम्पूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण मन ही मन हर्षित होते हुए, मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले।
देखिहउँ जाइ चरन जल जाता। अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ।
जे पद परसि तरी रिषि नारी। दण्डक कानन पावनकारी ।
जे पद जनकसुताँ उर लाए । कपट कुरंग संग घर धाए ।
हर उर सर सरोज पद जेई । अहोभाग्य मैं देखिहउँ तेई ।
दोहा- जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ ।
ते पद आजु बिलोकिहउँ । इन्ह नयनन्हि अब जाइ 1142।।
वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुन्दर कमल चरणों के दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं।
जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गयी और जो दण्डक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है और जो चरण कमल साक्षात् शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में बिराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज में देखूँगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अहा! आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर देखूँगा।
एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा। आयउ सपदि सिन्धु एहिं पारा।
कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा। जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा ।
ताहि राखि कपीस पहिं आए । समाचार तब ताहि सुनाए ।
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई ।।
इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जहाँ श्री रामचन्द्र जी की सेना थी, आ गये। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि यह शत्रु का कोई खास दूत है, उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आये और उनको सब समाचार कह सुनाया।
हस्ती साठ सहस्त्र बल, सदा धर्म की सींव ।
सदा श्वेत ध्वज सोहते, यह राजा सुग्रीव ॥
सुग्रीव में साठ हजार हाथियों का बल था। सुग्रीव ने भगवान राम के पास जाकर कहा- हे रघुनाथ जी ! रावण का भाई विभीषण, आपसे मिलने आया है और मैंने उसे वहीं पर रोक दिया है, उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है?
कह प्रभु सखा बूझिऐ काहा । कहइ कपीस सुनहु नर नाहा ।
जानि न जाइ निसाचर माया । काम रूप केहि कारन आया ।।
तब भगवान राम कहते हैं कि हे मित्र! तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? तब बानर राय सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ! राक्षसों की माया जानी नहीं जाती यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली, न जाने किस कारण आया है।
भेद हमार लेन सठ आवा । राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ।।
जान पड़ता है कि यह दुष्ट हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बाँध रखा जाये।
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारि । मम पन सरनागत भयहारी ।।
तब भगवान राम ने कहा- भैय्या! तुम हमारे सखा हो, राजा होने के नाते, तुमने भली नीति विचारी है, करना तो यही उचित है, तुम्हारी यह सलाह हमारे हित के लिए उपयोगी ही है, हम इसका खण्डन नहीं करते, परन्तु भाई! मेरा प्रण क्या है यह भी तुमसे छिपा नहीं है, शरण में आये हुए की रक्षा करना कर्त्तव्य है। अपने जीवन में, जो एक बार भी कह देता है कि प्रभो! मैं तेरा हूँ तो मैं उसे सारे संसार से अभय कर देता हूँ, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है।
दोहा- सरनागत कहुँ जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि ।
ते नर पावर पापमय, तिन्हहिं बिलोकत हानि ।। 43।।
जो कोई अपने अहित का अनुमान करके शरण में आये हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर, क्षुद्र, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी पाप लगता है।
कोटि बिप्रबध लागहिं जाहू । आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू ।
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥
जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
भगवान से जीव का विमुख होना पाप है, क्योंकि जीव से पाप तभी होता है जब वह भगवान से विमुख हो जाता है। विमुख होने पर जीव और जहाँ सन्मुख हुआ कि वह फिर जीव न रहा, फिर तो वह शिब (भगवान) ही है। जब जीव न रहा, तब पाप भी न रहे।
डण्डा, अपने को डण्डा मानता है यही उसका लकड़ी से विमुख होना है और यदि डण्डा अपने को लकड़ी जानता है तो यही उसका लकड़ी से सन्मुख होना है, इसी तरह जब अपने आपको जीव मानता है, तब यही भगवान से विमुख होना है और जब अपने आपको भगवान आत्मा जानता है, तब यही भगवान के सन्मुख होना है। भगवान से विमुख होने पर जीव आवागमन में फँसता है और सन्मुख होने पर जीव का आवागमन मिटता है, इस पर श्वेताश्वरोपनिषद् की एक श्रुति आती है, जिसमें जीव के आवागमन के कारण और उससे छूटने का उपाय बताया गया है।
सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ।
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥
(श्वेता.उ.अ-1 मं-6)
अर्थात् सर्व के प्रेरक भगवान को अपने आपसे भिन्न मानकर अनादि काल से हंस जीव, ब्रह्मचक्र यानि संसार में भ्रमता रहता है और जब भगवान एवं अपने आ 'मैं' को शरीर से भिन्न करके एकता का अनुभव करता है तब वह तत्काल ही, समस्त बन्धनों से मुक्त होकर अमृतत्व पद (कैवल्य पद) को प्राप्त हो जाता है। भगवान से अपने आप को भिन्न मानना, यही भगवान से अलग होना है और जीव का यही आवागमन का कारण है और जब भिन्न मानना छोड़ देता है अर्थात् भगवान से अपने आपको अभिन्न जानता है तब वह भगवान से जुड़ जाता है, उसका आवागमन मिट जाता है। श्रुति कहती है -
प्रकृतिविकृतिभिन्नः शुद्धबोधस्वभावः सदसदिदमशेषं भासयन्निविशेषः ।
विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववस्था स्वहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः ॥
(वि.चू.-137)
अर्थात् भगवान किसी का न कार्य है, न कारण है, वह शुद्ध बोध स्वरूप है अर्थात् परात्पर मायातीत है। अपने आपको कुछ मान लेना, यह अशुद्ध बोध है और अपने आपको जैसा है, वैसा ही जान लेना (बिना मान्यता के) यह शुद्ध बोध है, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में विलास करता है अर्थात् इनको जानता है, वही अपने आपको 'मैं' हूँ 'मैं' हूँ रात-दिन कहते रहता है, यह आत्म बोधक शब्द है, भाववाचक है, ब्रह्म वाचक है, देह वाचक शब्द नहीं है।
जिज्ञासुओं! ऐसा निश्चय करो, इसका अनुभव करो -
'मैं' उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, यही राम है, भगवान है, जिसकी अनुभूति रोज करायी जाती है, परन्तु यह समझ में तभी आता है, इसकी अनुभूति तभी होती है जब हृदय सन्मुख होता है, हम बड़ी सरलता से समझा रहे हैं, ध्यान से समझो - देखो भैय्या! जो भाव हमेशा न रहे उसे प्रपंच कहते हैं और जो भाव सर्वकालीन है, बस! वही भगवान है।
'मैं' देह हूँ, 'मैं' स्त्री हूँ, 'मैं' पुरुष हूँ, 'मैं' जीव हूँ ऐसा कहा जाता है, तब देह भाव, स्त्री भाव, पुरुष भाव, जीव भाव आदि 'मैं' के बाद जो भाव है, वे सब भाव जागृत अवस्था में ही रहता है, मान लो स्वप्न अवस्था में ही रहता है, परन्तु क्या गाढ़ी नींद, सुषुप्ती अवस्था में भी यह भाव रहता है? उत्तर होगा नहीं, वहाँ सर्व भावों का सर्वथा अभाव रहता है। बस, यही भाव जिसका अभाव रहता है, वही प्रपंच है। परन्तु, 'मैं' आत्मा, चेतन तत्त्व तो रहता हूँ, उसका अभाव तीनों काल और तीनों अवस्थाओं में कभी भी नहीं होता, इसलिए यही सचाई है कि 'मैं' ही सर्वकालीन हैं, इसलिए इसे जानो, पकड़ो, इसका अनुभव करो।
भगवान राम कहते हैं कि -
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा ।।
मेरे दर्शन का यही प्रत्यक्ष फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप (स्वाभाविक भाव) को प्राप्त कर लेता है, इससे पता चलता है कि जीव का सहज स्वरूप जीव नहीं है, जीव तो काल्पनिक है, माना हुआ है, जीव का सहज स्वरूप तो भगवान आत्मा है, राम है, सच्चिदानन्द है।
महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि -
करम बचन मन छाड़ि छलु जब लगि जनु न तुम्हार ।
तब लगि सुख सपनेहुँ नहीं, किएँ कोटि उपचार ।।
(अ.का. दोहा 107)
मन, वचन और कर्म के छल को जब तक कोई नहीं त्यागता, तब तक वह तुम्हारा जन अर्थात् तुम्हारा भक्त नहीं हो सकता और इस स्थिति में उसे स्वप्न में भी सुख, शांति नहीं मिल सकती, चाहे वह करोड़ों उपाय क्यों न करे। अब भगवान राम के प्रति मन, वचन और कर्म का छल क्या है-विषय समझो-
देखो ब्राह्मण पिता से पुत्र होगा वह ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र नहीं होगा, परन्तु यदि कोई ब्राह्मण पुत्र अपने को मन से अन्य जाति का मानता है तो यह हुआ उसके मन का छल। वाणी से ब्राह्मण न बताकर यदि वह पूछने पर अपने को अन्य जाति का बताता है तो यह हुआ उसके वाणी का छल और यदि वह कर्म भी ब्राह्मण का न करके अन्य जाति का कर्म करता है तो यह हुआ उसके कर्म का छल, तो फिर ऐसे पुत्र पर क्या ब्राह्मण पिता प्रसन्न होगा? कदापि नहीं, इसी तरह भगवान राम जब परम पिता हैं और हम उनकी संतान हैं, पुत्र हैं, तब राम चराचर के अस्तित्व का जो पुत्र होगा, वह पिता की जाति का ही होगा, अन्य जाति का नहीं। देखो! राम की जाति समझो -
राम सच्चिदानन्द दिनेसा ।।
राम, सत्, चित्, आनन्द स्वरूप, अखण्ड, अजन्मा, अकर्त्ता है, व्यापक है, तब उसका पुत्र भी उसी जाति का होगा। जो जाति पिता की, वही जाति पुत्र की होती है, क्योंकि वह पिता की ही जाति का तो है, आत्मा, सत्, चित्, आनन्द, स्वरूप, अखण्ड, अजन्मा, अकर्त्ता और व्यापक है, परन्तु वह अपने आपको आत्मा न जानकर, आत्मा न बताकर, मन से वह अपने को साढे तीन हाथ का शरीर मानता है, जन्म-मरण वाला मानता है, सुखी-दुखी, कर्त्ता-भोक्ता मानता है तो यह हुआ उस पुत्र का मन का छल और वाणी से भी यही औरों को बताता है कि मैं देह हैं, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जीव हूँ आदि। तो यह हुआ उस पुत्र का वाणी का छल और भगवान राम अकर्ता, ब्रह्म हैं, परन्तु उसका पुत्र होते हुए स्वयं अकर्त्ता होते हुए अपने को कर्त्ता, भोक्ता मानता है, सुखी-दुःखी मानता है तथा कर्त्तापने और भोक्तापने के अहंकार को लेकर कर्म करता है तो यह उसके कर्म का छल हुआ, तब भला परमपिता राम ऐसे कुल कलंकी पुत्र पर क्या कभी प्रसन्न होने वाला है? कदापि नहीं।
जीव वेश्या का पुत्र है, इसका कोई खास पिता नहीं गंगा गये गंगादास, यमुना गये यमुनादास। यही सब भगवान राम के प्रति मन, वचन और कर्म से छल करना है।
किसी को पूछने पर कि तुम कौन हो, तब अपने आप को शरीर बताना, स्त्री, पुरुष बताना (यद्यपि वह आत्मा है) यह अपना गलत हुलिया बताना है, यह दफा 468 का जुर्म है, इसके लिए सजा है "जन्म और मरण'। अपने आपको आत्मा न बताकर मैं संसारी जीव हूँ बताना, यह गलत हुलिया बताना है, इसकी सजा है, चौरासी लाख योनियों में 'आवागमन'। अतः, 'मैं' के ऊपर जितनी मान्यताएँ हैं, वे ही सब करोड़ों जन्म के पाप हैं, जो भगवान राम के सन्मुख होते ही नष्ट हो जाते हैं। मन, वचन, कर्म से जब छल रहित हो गया, तब फिर क्या रहा? "निर्मल मन" अर्थात् भगवान ही, भगवान रह गया। भगवान कहते हैं -
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।।
नदी जब तक छल रहित नहीं हो जाती, तब तक वह समुद्र को प्राप्त नहीं होती। नदी का अपने नाम रूप का त्याग कर देना ही, समुद्र के प्रति उसका छल रहित होना है। इसी तरह नाम रूप का जब तक त्याग नहीं हो जाता, सर्व-मान्यताओं का अभाव नहीं हो जाता, तब तक राम से मिलना नहीं हो सकता। बस, यही राम के सन्मुख होना है। जो जैसा है उसे वैसा ही न जानकर कुछ का कुछ मानना, अरे! यही तो पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। शुभाशुभ कर्मों के कर्त्तापने और भोक्तापने का जो अहंकार है यही जीव का पाप है और उसी पाप के कारण न जाने कब से यह जीव चौरासी लाख योनियों में भटकता फिर रहा है।
अब कर्म क्या है? समझो -
जो किया जाये उसे कर्म कहते हैं। पहिले कर्त्ता, फिर कर्म, इसके बाद क्रिया होती है। अब प्रश्न होता है कि 'मैं' कर्म है या कर्त्ता? उत्तर है 'मैं' कर्ता है और 'हूँ' क्रिया है। मैं कर्ता और हूँ क्रिया के बीच में जो कुछ भी है, वे सभी कर्म हैं।
मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जीव हूँ, इनमें मैं और हूँ के बीच में देह, पुरुष स्त्री और जीव ये सब हैं। ये सब कर्म हैं, देहभाव, पुरुष भाव, स्त्री भाव, जीव भाव इन सब भावों का अभाव कर दो अब शेष रह गया, केवल 'मैं' हूँ। वस! यही भगवान है, इस भाव में कर्मों का अत्यन्ताभाव हो गया, सर्व पापों का अभाव हो गया, 'मैं' हूँ, यही राम है, भगवान देश है, आत्म देश है, यहाँ जीव देश का विधान नहीं रह जाता, यहाँ कर्म, धर्म, विधि, निषेध कुछ नहीं है, केवल अपना आप है।
पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ।
जौं पै दुष्ट हृदय सोइ होई । मोरें सनमुख आव कि सोई ॥
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।
भेद लेन पठवा दससीसा । तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥
जग महुँ सखा निसाचर जेते। लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ।
जौं सभीत आवा सरनाई । रखिहउँ ताहि प्रान की नाई ॥
भगवान राम कहते हैं पापी का सहज स्वभाव है कि वह मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता अर्थात् आत्मा के सन्मुख आ ही नहीं सकता, अगर जीव वस्तुतः जीव है तो वह कभी भगवान हो ही नहीं सकता। हे सखा सुग्रीव! यदि विभीषण भेद लेने ही आया हो तो कोई बात नहीं न इसके लिए कोई भय है न हानि, क्योंकि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण संसार के सब राक्षसों को पल मात्र में नाश कर सकने में समर्थ है। इसलिए, उसे आने दो, चिंता मत करो और यदि भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा।
दोहा - उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपा निकेत ।
जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ||44||
भगवान राम की इस आज्ञा को सुनकर हनुमान समेत, अंगद और सुग्रीव सभी बड़े प्रसन्न हुए और कृपालु भगवान राम की जय हो, कहते हुए चले।।
सादर तेहि आगे करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर ।
दूरिहि ते देखे द्वौ भ्राता । नयनानंद दान के दाता ।।
बहुरि राम छबि धाम बिलोकी। रहेउ ठटुकि एकटल पल रोकी ।
भुज प्रलंब कंजारून लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचन ।।
सिंघ कंध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन मोहा ।
नयन नीर पुलकित अति गाता। मन घरि धीर कही मृदु बाता ।।
विभीषण को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले, जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनन्द का दान देने वाले, अत्यन्त सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर ही से देखा। शोभा के धाम भगवान राम को देखकर, पलक मारना रोककर, ठिठक कर, स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गये। भगवान की विशाल भुजाएँ हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला साँवला शरीर है। सिंह जैसे कंधा है, विशाल वक्षस्थल (चौड़ी छाती) अत्यन्त शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला, मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया, फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने बड़ी दीनतापूर्वक कोमल वचन कहे -
नाथ दसानन कर मैं भ्राता । निसिचर बंस जनम सुरत्राता ।
सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकहिं तम पर नेहा ।।
भाई! जब बड़ों के पास जाओ, तब उनके बिना पूछे अपना परिचय देना पड़ता है, यह शिष्टाचार है। विभीषण कहते हैं कि हे नाथ! मैं वही दशानन का भाई हैं, जिसने माता बैदेही का हरण किया है। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है।
दोहा - श्रवन सुजसु सुनि आयउँ, प्रभु भंजन भव भीर ।
त्राहि-त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर ||45||
मैं कानों से आपका सुयश सुनकर, मुमुक्षु की भाँति, आपकी शरण में आया हूँ। आप जन्म-मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुःख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले, श्री रघुबीर! मेरी रक्षा कीजिये! हे शरण! सुखद रघुबीर, हे आरत हरण! ये तमाम सम्बोधन राम के लिए है, विभीषण कहते हैं कि हे भव भीर भंजन! आपका सुन्दर यश कान से सुनकर मैं शरण में आया हूँ। हे नाथ! मेरी रक्षा कीजिये! मेरी रक्षा कीजिये !
अस कहि करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा ।।
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हृदयें लगावा ।।
अनुज सहित मिलि ढ़िग बैठारी। बोले बचन भगत भयहारी ।।
कहु लंकेस सहित परिवारा। कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ।।
प्रभु ने ऐसा कहकर दण्डवत् करते देखा तो वे अत्यन्त हर्षित होकर तुरंत उठे, उन्हें विभीषण के दीन वचन बड़े प्रिय लगे, भगवान राम ने उन्हें अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि हे लंकेश! अभी सेतु बंधा नहीं, लंका पर चढाई हुई नहीं, रावण मरा नहीं और विभीषण को भगवान में लंकेश की उपाधि से विभूषित कर दिया अर्थात् उसे लंका का राज्य मिल गया, शरणागत का यह तत्काल प्रत्यक्ष फल है।
भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि हे लंकेश ! परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा रहना बुरी जगह पर है।
खल मंडली बसहु दिनु राती । सखा धरम निबहइ केहि भाँती।
मैं जानऊँ तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती ॥
बरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता ।
अब पद देखि कुसल रघुराया। जौं तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥
भगवान राम कहते हैं, हे सखे ! दिन-रात तुम दुष्टों की मण्डली में बसते हो, तुम्हारा धर्म किस तरह निभता है, मैं तुम्हारा सब आचार-व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यन्त नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती।
हे तात! नरक में रहना भले ही पड़ जाये, पर विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण ने कहा- हे रघुनाथ जी ! अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की।
दोहा - तब लगि कुसल न जीव कहुँ, सपनेहुँ मन विश्राम।
जब लगि भजत न राम कहुँ, सोक धाम तजि काम ||46||
तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक कि वह शोक के घर कामनाओं, वासनाओं का त्याग न कर दे और भगवान राम को न भजे। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि हृदय में भगवान राम का निवास न हो जाये। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग-द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि, तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक हे नाथ! आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता।
अब मैं कुसल मिटे भय भारे । देखि राम पद कमल तुम्हारे ।
तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिबिध भव सूला ।।
मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ।
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। तेहिं प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा ।।
दोहा - अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज ।
देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद कंज ||47||
विभीषण ने कहा- हे नाथ! आपके श्रीचरणों के दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ, मेरे भारी भय मिट गये। हे कृपालु ! आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उन्हें तीनों प्रकार के भव-शूल नहीं व्यापते। मैं अत्यन्त नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज ! मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिवजी के द्वारा सेवित युगल कमलों को अपने नेत्रों से देखा।
सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ।
जौं नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोहीं ।॥
तजि मद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना ।
जननी जनक बन्धु सुत दारा । तनु घनु भवन सुहृद परिवारा ।।
सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहिं बाँध बरि डोरी ।
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥
अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसइ धनु जैसे ।
तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे । घरउँ देह नहिं आन निहोरे ।।
दोहा-सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ।
तें नर प्रान समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम ।।48।।
भगवान राम ने कहा- हे सखा ! सुनो मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काग भुशुण्डी, शिवजी और पार्वती जी जानती हैं। कोई मनुष्य चराचर का द्रोही भी क्यों न हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आता है और मद, मोह तथा नाना प्रकार के छल-कपट को त्याग देता है तो मैं उसे अतिशीघ्र साधु के समान कर चिता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार इन सबकी नमता को बटोरकर डोरी बटकर जो मेरे चरणों में बाँध लेता है अर्थात् सबका केन्द्र मुझे ही बना लेता है तथा जो समदर्शी है जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन, मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे-लोभी के हृदय में धन बसा करता है और हे भाई! तुम सरीखे सन्त ही मुझे प्रिय है और मैं किसी के लिए देह धारण नहीं करता, मेरे देह धारण करने का यही कारण है।
जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं।
सुनु लंकेस सकल गुन तोरे । ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ।
राम बचन सुनि बानर जूथा। सकल कहहिं जय कृपा बरुथा ।।
हे लंकेश ! सुनो तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। भगवाम राम के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्रीराम की जय हो ।
सुनत बिभीषनु प्रभु कै बानी। नहिं अघात श्रवनामृत जानी ।
पद अंबुज गहि बारहिं बारा। हृदय समात न प्रेमु अपारा ॥
सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ।
उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ।।
अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी ।
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । मागा तुरत सिन्धु कर नीरा ॥
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥
अस कहि राम तिलक तेहि सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा ।।
विभीषण, भगवान की इन अमृतमयी वाणी को सुनते अघाते नहीं, वे बार-बार भगवान के चरणों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम हृदय में नहीं समा रहा है। वे कहते हैं- हे चराचर के स्वामी! हे शरणागत रक्षक!! हे अन्तर्यामी प्रभु! मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गयी। अब तो हे कृपालु! शिवजी के मन में सदैव प्रिय लगने वाली, अपनी पवित्र भक्ति ही मुझे कृपा कर दीजिये। भगवान श्रीराम ने 'एवमस्तु' ऐसा ही हो, कहकर तुरन्त ही समुद्र जल मांगा और कहा -
हे सखा! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परन्तु जगत् में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता, ऐसा कहकर भगवान राम ने उनको राजतिलक कर दिया, जिसे देख आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई।
दोहा - रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड ।
जरत बिभीषनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ||49||
रावण का क्रोध प्रचण्ड अग्नि थी, जिसमें विभीषण जल रहा था, उस जलते हुए विभीषण की भगवान राम ने रक्षा की और उसे अखण्ड राज्य दिया।
दोहा - जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ।
सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ।।49 ख।।
भगवान शिव की तपस्या कर रावण ने अपने दशों सिरों की बलि चढ़ाकर जिस बड़ी से बड़ी सम्पत्ति को प्राप्त किया था। भगवान राम ने उसी सम्पत्ति को बड़े संकोच के साथ विभीषण को दिया। भाव यह कि भगवान सोच रहे हैं कि अरे! कुछ नहीं दिया जा रहा है, इससे भी अधिक देना था। बस, यहीं पर विभीषण शरणागति का उपसंहार है।
भगवान कहते हैं -
जो महापुरुष निरपेक्ष है, शांत है, सर्वमान्यताओं से रहित है, निबैर है, समदर्शी है तथा सर्व के प्रिय है, ऐसे महापुरुष के पीछे-पीछे मैं घूमता रहता हूँ ताकि उनके चरणों की धूल उड़-उड़कर मुझ पर लगती रहे और मैं कृतार्थ होता रहूँ।
4. वेद स्तुति
अभी का प्रसंग है उत्तरकाण्ड के अंतर्गत वेदों द्वारा स्तुति, गोरखपुरी रामायण दोहा नं. 12वाँ -
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम ।
बंदी बेष बेद तब आए जहँ श्रीराम ।।12 ख।।
प्रभु सर्बग्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान ।
लखेउ न काहूँ मरम कछु लगे करन गुनगान ।।12 ग।।
भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो चुका तब सब देवता वहाँ आये और अलग- अलग स्तुति करके वे सब अपने-अपने लोक को चले गये। इसके बाद, भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आये, जहाँ श्रीरामजी थे।
कृपानिधान सर्वज्ञ प्रभु राम ने उन्हें पहचानकर उनका बड़ा आदर किया, परन्तु इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुण गान करने लगे -
छन्द -
जय सगुन निर्गुन रूप-रूप अनूप भूप सिरोमने ।
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुजबल हने ।।
अवतार नर संसार भार विभंजि दारुन दुख दहे ।
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ।।1।।
तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे ।
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ।।
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि दुख ते निर्बहे ।
भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे ।।2।।
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी ।
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ।।
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे ।
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे ।।3।।
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरि ।
नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ।।
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे।
पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ।।4।।
अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने ।
षट कन्ध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने ॥
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे ।
पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे ।।5।।
जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं ।
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ।।
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागहीं ।
मन बचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ।।6।।
वेदों ने भगवान राम की इस प्रकार स्तुति की और वे अन्तर्धान हो गये और ब्रह्म लोक को चले गये।
दोहा- सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार ।
अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥13-क।।
भाई! वेदों द्वारा यह जो स्तुति की गयी उसमें से अब, पांचवें श्लोक की चारों पंक्तियों की व्याख्या होगी "अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने से लेकर संसार बिटप नमामहे" तक की। पहले इस छन्द का शब्दार्थ सुनो-वेद शास्त्रों ने कहा है कि संसार वृक्ष का मूलाधार अव्यक्त है अर्थात् जिस तरह पृथ्वी पर वृक्ष जमता है (यदि पृथ्वी न हो तो वृक्ष रहेगा कहाँ? तब वृक्ष का आधार पृथ्वी हुई) इसी तरह यह जो संसार वृक्ष है, उसका मूल (आधार) 'अव्यक्त' है। फिर अनादि है। वृक्ष में छाले हैं ऐसा 'निगमागम भने' वेद शास्त्रों ने कहा है।
इस संसार वृक्ष के छः स्कन्ध हैं (पेड़ में जहाँ से डालियाँ फूटती हैं, उसे स्कन्ध कहते हैं)। पच्चीस शाखाएँ (डालियाँ) हैं, ये डालियाँ सब दिशाओं में फैली हैं। इनमें अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, इस वृक्ष में दो फल हैं कटु और मधुर अर्थात् एक फल कडुवा है और दूसरा मीठा। एक बेलि है अर्थात् लता है, जो इस संसार रूपी वृक्ष की ही आश्रित है। अन्य वृक्ष तो अपनी-अपनी ऋतुओं में ही फलते-फूलते हैं,
परन्तु यह 'संसार वृक्ष' 'पल्लवित फूलत नवल नित' नित्य हरा-भरा, लहलहाते रहता है तथा इसमें नित्य फूल और फल लगते रहते हैं। ऐसे इस संसार वृक्ष को हम नमस्कार करते हैं, यह हुआ इस छन्द का शब्दार्थ, अब इसका भावार्थ सुनो - इस संसार वृक्ष का मूल अर्थात् आधार जो है वह अव्यक्त है, अनादि है। अण्डज, पिण्डज, उद्भिज और स्वेदज ये चार खानि इस वृक्ष की त्वचा अर्थात् छाल हैं। शब्द, स्पर्श, रूप रस और गन्ध ये पाँच विषय और छठवां मन यही छह इस संसार वृक्ष के स्कन्ध हैं और हर एक विषय के (एक-एक विषय के, पाँच-पाँच) तन्मात्राएँ (ऐसे पच्चीस तत्त्व से ही) इस वृक्ष की शाखाएँ अर्थात् डालियाँ हैं। अनन्त वासनाएँ ही इससे अनेक पत्ते हैं। शुभाशुभ कर्म ही इसके अनेक फूल हैं। सुख और दुःख ये दोनों ही, इसके कटु और मधुर अर्थात् कडुवा और मीठा ये दो फल हैं। वासना रूपी एक ही बेलि है, जो इस वृक्ष से लिपटी हुई इसकी आश्रित है, जो हमेशा फूलती-फलती रहती है। यह हुआ उसका भावार्थ अब इनकी हर एक की अलग-अलग व्याख्या सुनो।
देखो-जो वृक्ष जितना ही बड़ा विशाल होता है, उसका बीज उतना ही छोटा और सूक्ष्म होता है। पीपल के ही वृक्ष को देखो, उसका वृक्ष कितना विशाल होता है, परन्तु उसका बीज उतना ही सूक्ष्म होता है, इसके एक फल में अनन्त बीज होते हैं, इसके बीज को देखकर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता कि इतने सूक्ष्म बीज के भीतर ऐसा विशाल वृक्ष समाया हुआ है, फिर एक ही वृक्ष नहीं अनन्त वृक्ष, यह उस सूक्ष्म बीज का चमत्कार है। अरे! वह बीज ही तो है इसके स्कन्ध, शाखा (डालियाँ) टहनियाँ, पत्ते, फूल और फल आदि होकर स्वयं इनमें समाया हुआ है।
गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि -
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।।
(अ. 7वां, श्लोक 10वीं)
हे अर्जुन! तू सम्पूर्ण भूतों का सनातन कारण मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ।
देखो, यदि वेदों ने इस पर संसार का विकल्प नहीं किया होता, तब तो यह साक्षात् भगवान ही है, परन्तु यहाँ वेदों ने संसार को वृक्ष की उपमा देकर भगवान का दिग्दर्शन कराया है। इस संसार वृक्ष का मूल अर्थात् जड आधार 'अव्यक्त' है। जो किसी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इसलिए अव्यक्त अथवा जो स्वयं व्यक्त न कर सके कि 'मैं' कैसा हूँ, इसलिए अव्यक्ता व्यक्त माने प्रगट और अव्यक्त माने अप्रगट अर्थात् जिसे वाणी न कह सके, दृष्टि जिसको देख न सके, चित्त जिसका चिन्तन न कर सके, मन जिसे मनन न कर सके, इसलिए अव्यक्त। तो वह कौन है जो किसी के द्वारा भी व्यक्त नहीं हो सकता? उत्तर है यह 'मैं' आत्मा ही हूँ।
वाणी को मैं कहता हूँ वाणी मुझे क्यों कहेगी, मन को बुद्धि को, चित्त को, इन्द्रियाँ आदि को मैं जानता हूँ, इन सबका साक्षी में हूँ ये सब मुझे क्या जान सकेंगे, इसलिए 'मैं' आत्मा ही अव्यक्त हूँ, श्रुति कहती है कि -
येनेद सर्व विजानाति तं केन विजानीयद्विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ।।
(वृह.2 / 4 / 14 )
जिससे यह सब जाना जाता है, उसको किससे जाने? अरे ! जानने वाले को जिससे जाने ? अर्थात् 'मैं' जिसको जानता हूँ वह, मुझको क्या जान सकेगा, इसलिए संसार वृक्ष का मूलाधार 'मैं' आत्मा अव्यक्त हूँ।
'मैं' स्वयं अपने को व्यक्त नहीं कर सकता, अपने आपको 'मैं' कहूँ कि 'मैं' ऐसा हूँ, तो अव्यक्त नहीं और यदि 'मैं' कहूँ कि जैसा हूँ तो व्यक्त नहीं, 'मैं' का अनुभव तो तुम कर रहे हो, अब अपना अनुभव बताओ कि 'मैं' जिसका कि तुम अनुभव कर रहे हो, कैसा है? तुम बता नहीं सकते कि 'मैं' ऐसा हूँ, केवल अनुभव किया जा रहा है, वह 'मैं' का अनुभव बताया नहीं जा सकता, यदि तुम कहते हो कि 'मैं' ऐसा हूँ, तो वैसा तुम हो नहीं, आकार-प्रकार वाला हूँ, सत् हूँ, असत् हूँ, व्यापक हूँ, अखण्ड हूँ, निराकार, साकार हूँ तो अव्यक्त नहीं, क्योंकि इसे वाणी व्यक्त कर रही है और 'मैं' आत्मा वाणी का विषय हूँ नहीं, इसलिए अव्यक्त और यदि कहते हो 'जैसा हूँ' तो जैसा कहने से वह 'मैं' आत्मा व्यक्त न हुआ, इसलिए 'मैं' आत्मा 'अव्यक्त'। विश्व में किसी की ताकत नहीं कि 'मैं' कैसा हूँ, यह बता सके, कह सके, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही क्यों न हो, सबको चुनौती है।
राम अतर्क्स बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी ।।
जिसके लिए तर्क नहीं किया जा सकता, जो मन से, बुद्धि से, वाणी से, अतर्क्स है। माता पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं कि 'मत हमार अस सुनहि सयानी' यह ऐरे-गैरे का मत नहीं है। यदि मैं अपने आपको व्यक्त करूँगा तो किसके द्वारा व्यक्त करूँगा। वाणी के द्वारा ही तो व्यक्त करूँगा, तो क्या वाणी अव्यक्त को व्यक्त करेगी? अरे! वाणी ही खत्म हो जायेगी, अव्यक्त हो जायेगी। इसी तरह मन, बुद्धि, चित्त, आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियाँ, जो भी उसे जानने चलेगा वह वही होकर उसे जान सकेगा, जो जैसा है उसे वही होकर जाना जाता है। अरे यार! चोर को पकड़ने के लिए उसे चोर होकर ही पकड़ना पड़ता है। सजातीय, सजातीय का मेल होता है। इसलिए अब 'मैं' आत्मा अव्यक्त हूँ तो मुझ अव्यक्त को जानने के लिए, अव्यक्त ही होकर जानना पड़ेगा।
इस अव्यक्त मुझ आत्मा, आत्म तत्त्व, आधार भूमि पर संसार है, जो कि अव्यक्त कहा गया। प्रश्न होता है कि जब संसार भी अव्यक्त है, तब संसार नाम क्यों पड़ा?
देखो विषय समझो- 'देह है' ये देह विकल्प ही संसार है, यह देह विकल्प 'है' अस्तित्व पर हुआ, बिना देह कहे यह जो भास रहा है, उस 'है' अस्तित्व को ही देह कह रहे हो तो यह 'है' अस्तित्व, भास ही आधार अर्थात् मूल हुआ। यदि यह भास 'है' अस्तित्व न होगा, तो देह कहोगे किसको? इसी तरह सारे चराचर का विकल्प अस्तित्व 'है' पर ही है। देह है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इत्यादि इस तरह जहाँ तक मन वाणी का विषय है वह सभी संसार है अर्थात् कुछ भी विकल्प करना, बस यही वृक्षारोपण है, ये सर्व विकल्प 'है' अस्तित्व, भगवान आत्मा 'मैं' पर ही है।
फिर कहते हैं 'अव्यक्त मूल मनादि' जरा समझना और समझ लिया तो मर गया। अरे! समझती कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि जहाँ खो जाती है यही तो मरना है, समझने के बाद क्या बुद्धि बची रहेगी? नहीं। बस, यही मरना है।
अरे भाई! जिसका आधार मूल और बीज ही जब अव्यक्त है तो फिर उसका वृक्ष भी अव्यक्त ही होगा, वही कैसे व्यक्त हो सकता है? तुम व्यक्त किसे कह रहे हो? अव्यक्त का क्या लक्षण है? अरे! जिसका कोई लक्षण नहीं वही अव्यक्त का लक्षण है, जिसका बीज ही 'मैं' आत्मा अव्यक्त अर्थात् अलक्षण हूँ तो फिर संसार वृक्ष का ही क्या लक्षण होगा? इसलिए यह भी अलक्षण ही है। जो पदार्थ 'ऐसा' हो, उसका लक्षण हो और जो 'जैसा' हो तो फिर वह लक्षण शून्य है, अलक्षण है। तो फिर जैसा 'मैं' अलक्षण वैसा संसार अलक्षण जैसे 'मैं' अचिन्त्य, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अदृष्ट हूँ, प्रत्ययसार हूँ, उसी तरह संसार भी, अचिन्त्य, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अदृष्ट, प्रत्ययसार है।
प्रश्न होता है तब फिर दिख क्या रहा है? दिखने वाला दिख रहा है या उसे जो देख रहा है, वह दिख रहा है। विषय सूक्ष्म है समझो, उत्तर है-उसे जो देख रहा है, वह दिख रहा है। तो, देखने वाला दृष्ट है या अदृष्ट है? उत्तर होगा-अदृष्ट है। और क्या वास्तव में दिख रहा है? जैसे 'देह'। यह देह क्या दिखता है? अरे, देह तो विकल्प है, जो है ही नहीं, अस्तित्व हीन, तब वह क्या दिखेगा? तब क्या दिख रहा है।
भाई! दिख कुछ नहीं रहा, केवल विकल्पाधार की अनुभूति हो रही है, जिस पर देह का विकल्प है, उसकी केवल प्रतीति हो रही है, यह दिखना देखने वाले की अपेक्षा से है अन्यथा दिखना कहाँ?
है सो नजर न आवही, नहीं सो प्रगट दिखाय ।
यह कौतुक तबही लखै, जब सद्गुरु मिल जाय ।।
यह तो गुरु कृपा से समझा जा सकता है।
जो दिखता है, वह दिखता है, 'मैं' दिखता हूँ, तब दिखता है।
यह रहस्य जो जान लिया, फिर दिखना कहाँ जो दिखता है।
जो दिख रहा है वह 'मैं' ही हूँ, तब 'मैं' देखने वाला जब अदृष्ट हूँ, तब उस अदृष्ट की दृष्टि में यह दिखने वाला ही, कैसे दृष्ट होगा? वह भी अदृष्ट ही है, इसलिए यह संसार भी अदृष्ट होते हुए अचिन्त्य है, अलक्षण है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है। इसलिए ही वेदों ने "संसार विटप नमामहे" कहा है। अरे! संसार नमस्कार करने योग्य कब होगा? जब संसार भगवान सिद्ध होगा, इसके पहिले यदि संसार नमस्कार करने योग्य होता तो फिर महात्मा लोग ठोकर मारकर इसका त्याग कैसे करते। इसलिए जब मुझ आत्मा के सारे लक्षण संसार में घटेगा, तभी यह भगवान आत्मा सिद्ध होगा और तभी यह नमस्कार करने योग्य होगा। संसार को संसार मानकर, संसार से वैराग्य है और संसार को भगवान जानकर संसार का बोध है। संसार मानने से दृष्ट, चिन्त्य, ग्राह्य, व्यवहार्य लक्षण वाला आदि होता है। परन्तु, संसार को भगवान जानकर नहीं, भगवान जानने पर संसार अलक्षण, अचिन्त्य, अदृष्ट, अव्यहार्य आदि रूप दिखाई देता है, अनुभव होता है। रज्जू को सर्प मानने से क्या सर्प के डसने से = विष चढेगा? नहीं। तो फिर इसी तरह 'मैं' अव्यक्त आत्मा को संसार मानने से क्या संसार दिखेगा नहीं तो फिर अदृष्ट ही तो है। मगर काल्पनिक जगत दृष्ट, चिन्त्य, व्यवहार्य, लक्षण है और वास्तविक जगत्, अदृष्टं, अचिन्त्यं, अव्यवहार्य, अलक्षणं है तो फिर जो इतना महान वृक्ष है, वह वृक्ष नहीं, बीज ही है, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अदृष्ट है, इसी तरह यह जो दिख रहा है, वह संसार नहीं है, 'मैं' भगवान अव्यक्त आत्मा ही हूँ। इस बोध में अब संसार नमस्कार करने योग्य हुआ। जब संसार का लक्षण 'मैं' आत्मा से भिन्न हो, तब तो और कोई दूसरा भाव संसार के लिए ढूँढो और जब जो लक्षण 'मैं' आत्मा का है वही लक्षण संसार का है, तब फिर संसार का ग्रहण और त्याग कहाँ? जब मैं संसार मानता हूँ तभी संसार के त्याग और ग्रहण का विकल्प होता है और शरीरादिक प्रपंच को जो देखता है उसे देखता हूँ तो संसार ही नहीं मिलता तो फिर उसका त्याग और ग्रहण ही कहाँ?
यदि संसार है तो 'है' ही है और नहीं है तो भी 'है' ही है। यदि विना बीज के वृक्ष सिद्ध हो जाय तब तो वृक्ष है और यदि बिना बीज के 'मैं' वृक्ष सिद्ध नहीं होता तो फिर बीज ही है-जिसका नाम वृक्ष है। इसी तरह बिना 'मैं' के यदि संसार सिद्ध हो जाय तब तो संसार, संसार है और यदि सिद्ध नहीं होता तो फिर 'मैं' ही हूँ, जिसका नाम संसार है। इस पर कबीर पंथी लोग शंका करते हैं कि साहेब! पहिले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ? इसी तरह पहिले शरीर हुआ कि कर्म हुआ?
उत्तर है- तो साहेब (यदि कोई कबीर पंथी यहाँ बैठे हों तो सुने) पहिले न शरीर हुआ, न कर्म। पहिले अज्ञान हुआ, जब अज्ञान हुआ तब अपने आपको माना शरीर, अब जब शरीर माना अर्थात् शरीर हुआ तब फिर उससे हुए कर्म, जब कर्म किया तब फिर शरीर हुआ, इस प्रकार कर्म और शरीर की श्रृंखला चल पड़ी। इसलिए सबसे पहिले अज्ञान हुआ। इसी तरह न पहिले बीज हुआ न वृक्ष, पहिले अज्ञान हुआ। पहिले विकल्प हुआ बीज और वृक्ष का। विकल्प निकाल दो तो न बीज और न वृक्षा
इसी तरह 'मैं' आत्मा को ही संसार मानकर देखने दिखने का विकल्प करता हूँ, परन्तु जब अनुभव करने चलता हूँ तो संसार ही नहीं मिलता और जब संसार ही नहीं मिलता तब देखने-दिखने का विकल्प ही कहाँ? अरे! यहाँ तक नहीं है कि न में बोल रहा हूँ और न तुम सुन रहे हो, परन्तु अव्यक्त देश से देखो तब, वह सिर्फ इतना ही कहते बनता है कि जो है, वह 'मैं' हूँ का भाव ही है। इसके आगे और कुछ कहते, सुनते नहीं बनता इस भाव के लिए और कोई इशारा नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न हो तब तो कोई इशारा हो? ये हुआ 'अव्यक्त मूल' की व्याख्या।
अब चलो अनादि का समझो - देखो, वेदों ने इसे अनादि कहा है, ये जो 'अनादि शब्द है वह बड़ा मार्मिक है, गूढ है, अनादि कहते ही यह अपने आप अजन्मा शिड हो जाता है, जिसका आदि अर्थात् शुरुआत ही न हो उसे अनादि कहते हैं, जिसका जन्म समय, जन्म कुण्डली न हो, यदि वह पैदा हुआ होता तो इसकी जन्म कुण्डली अवश्य होती कि इस संसार को इतने लाख, इतने करोड़ वर्ष हुए, परन्तु ऐसा नहीं है। इसलिए ही यह अनादि है। मानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत माता कौशल्या ने भी चित्रकूट दरबार में माता सुनयना से इस संसार प्रपंच को अनादि कहा है-वे कहती हैं कि-
देबि मोह बस सोचिअ बादी। बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी ।।
इसलिए, संसार न तो स्वयं पैदा हुआ और न किसी ने इसे पैदा किया। संसार में कोई भी हो आ जावे मैदान में और इस देह को ही सिद्ध करके दिखावे कि यह पैदा हुआ है, अरे! देह क्या संसार की किसी भी वस्तु को ले लो उसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती।
स्वतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते ।
सदसत्सदसद्वापि न किं चिद्वस्तु जायते ॥
(गौ.पा. कारिका 4/22)
अर्थात् न सत् की उत्पत्ति होती है न असत् ही उत्पन्न होता है और न सत्- असत् दोनों की ही उत्पत्ति होती है। यदि सत् पदार्थ की उत्पत्ति मानोगे तो उत्पन्न हुआ, पदार्थ नाशवान होता है, फिर इसे सत् कैसे कहेंगे? क्योंकि, सत् वस्तु त्रिकाला बाध्य होती है और यदि असत् की उत्पत्ति मानोगे तो असत् बन्ध्यापुत्रवत् होता है अर्थात् जो है ही नहीं वह पैदा क्या होगा। तात्पर्य यह कि किसी प्रकार से भी किसी भी देश, काल, वस्तु का उत्पन्न होना किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता।
1. प्रत्यक्ष प्रमाण, 2. अनुमान प्रमाण, 3. श्रुतिशास्त्र प्रमाण एवं 4. स्वानुभूति प्रमाण। इन चारों प्रमाणों से जो सिद्ध हो, वही न्याय है और वही सार्वभौम सिद्धान्त है। दूसरी चीज यह है कि सत्, असत् दोनों का यदि जन्म माना जाये तो माया देश में है। माया का अधिष्ठान आत्म देश में नहीं है, क्योंकि माया का अर्थ होता है, अज्ञान, याने सत् का जन्म नहीं, सत् के अज्ञान देश में सत् का जन्म है। असत् देश में असत् का जन्म नहीं, असत् के अज्ञान देश में असत् का जन्म है। इसी तरह सत्, असत् देश में सत्, असत् का जन्म नहीं, बल्कि सत्, असत् के अज्ञान देश में सत्, असत् का जन्म माना जा सकता है। जैसे- रज्जू का सर्प रज्जू देश में न सत् है, न असत् है और न सत्- असत् दोनों है। रज्जू के अज्ञान देश में सर्प सत् भी है, असत् भी है और सत्, असत् दोनों भी है।
भैय्या! यह अध्यात्म है, कोई बाजारू चीज नहीं है, जो सबकी समझ में आ जाय। इस एक छन्द में ही सारी रामायण भरी हुई है। इस पर महीनों बोला जा सकता है।
तो फिर यह क्या है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है? अरे! 'मैं' ही हूँ, संसार-फंसार, देह-फेह कुछ नहीं है। चलो बच्चा आगे -
पढ़ना-लिखना बह्मन का काम, भजले बच्चा सीता-राम ।।
अब आगे 'तरु त्वच चारि' की व्याख्या सुनो-अण्डज, पिण्डज, उद्भिज और स्वेदज ये चार खानि इस संसार वृक्ष की त्वचा हैं अर्थात् छाल हैं।
अण्डज- अण्डा से पैदा होने वाली सृष्टि।
पिण्डज- रज-वीर्य से पैदा होने वाली सृष्टि।
उद्भिज - धरती से पैदा होने वाली सृष्टि, पेड़-पौधे।
स्वेदज- पसीने से पैदा होने वाली सृष्टि खटमल, पिस्सू आदि, यही चार खानि है।
षट्कन्ध शाखा - पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और छठवाँ मन ये ही छह स्कन्ध हैं, जहाँ से वृक्ष में शाखाएँ निकलती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पाँचों विषयों के हर एक विषय के पाँच-पाँच तन्मात्राएँ, ऐसे पच्चीस तत्त्व, प्राणादि ये ही इस संसार वृक्ष की शाखाएँ अर्थात् डालियाँ हैं, जो सब दिशाओं में फैली हुई हैं। अनन्त वासनाएँ ही इसके अनेक पत्ते हैं। जितने शुभाशुभकर्म हैं, वे ही फूल हैं। जिन पुण्य-पाप कमों की कोई गिनती नहीं, ये फूल घने हैं अर्थात् बहुत हैं। इन फूलों से सिर्फ दो प्रकार के ही फल फलते हैं, पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुःख, ये ही दो फल हैं। सुख-दुःख अनेक नहीं होता वह एक ही है, मगर जिस फूल से ये निकलते हैं वह एक नहीं है, वह अनेक है। क्योंकि, अनेकों पुण्य और अनेकों पाप हैं, परन्तु फल दो प्रकार के ही हैं सुख और दुःख। इन दोनों फलों का स्वाद अलग-अलग है, एक मीठा है वह सुख है, दूसरा कडुवा है वह फल दुःख है, क्योंकि फल दो ही है 'फल युगल' कहा है।
इस संसार रूपी वृक्ष पर एक ही 'बेलि' अर्थात् लता है जो इस वृक्ष के आश्रित है इससे लिपटी हुई है 'बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे' वह है 'वासना'।
विद्या, वनिता, वनलता, ये न गिनै कुल जात ।
जो समीप इनके बसै, ताही पै लपटात ॥
विद्या यह नहीं देखती कि यह किस जाति वर्ण का है। मैं इसके पास जाऊँ या न जाऊँ, वह तो जिसको अपने पास पाती है अर्थात् जो इसके समीप होता है उसी से वह लिपट जाती है। इसी तरह वनिता (स्त्री), वह जिसे समीप में पाती है चाहे वह किसी भी कुल जाति का क्यों न हो उससे वह लिपट जाती है। (यह कथन सार्वभौम नहीं है)।
नागिन डसती है तो एक ही बार जहर चढ़ता है, परन्तु इस नागिन के तो स्मरण मात्र से ही जहर चढ़ता है, इसलिए विवेकीजनों को इनसे विशेष सावधान रहना चाहिए 'मैं' हूँ, इस भावना के सिवा यदि कोई अन्य भावना न हो तो शायद ही यह जहर न चढ़े, नहीं तो बड़ी मुश्किल है और इस जमाने में तो और भी कठिन है, यही हालत बनलता का है, वह अपने समीप में जो भी वृक्ष पाती है, बस उसी से लिपट जाती है।
भैय्या! इस संसार वृक्ष के ऊपर एक ऐसी बेलि लिपटी हुई है, जिसका नाम बासना है। इसका अर्थ है कि जिसको तुम पाने की इच्छा करते हो, उसका यहाँ बास अर्थात् गन्ध तक नहीं है, वस्तु का होना तो दूर है।
इस संसार वृक्ष का कभी पतझड़ नहीं होता यह तीसों दिन, बारहों महीने, नित्य हरा-भरा रहता है। इसलिए "पल्लवत, फूलत नवल नित" कहा गया है।
यही तो संसार वृक्ष की शोभा है।
आज गरीबी है तो कल अमीरी है, आज बन्ध है तो कल मोक्ष है। आज जन्म है तो कल मरण है। आज योग है तो कल वियोग है। आज दुःख है तो कल सुख है। आज बीमार है तो कल आराम है। हर दिन एक-सा नहीं होता, आज कोई दाने-दाने को तरस रहा है तो कोई मौज से गुलछरें उड़ा रहा है। भाई! इसी का नाम संसार है। कोई कभी यह न समझे कि आज हम धनवान हैं तो हम सदा धनवान ही रहेंगे। आज हम पुत्रवान हैं तो सदा पुत्रवान ही रहेंगे। यहाँ बनना-बिगड़ना, जीना-मरना, हँसना- रोना, नित्य बना रहता है, यहाँ इसकी कभी कमी नहीं है।
दुनियाँ के जो मजे हैं, हरगिज ये कम न होंगे ।
चरचे यही रहेंगे, अफ़सोस हम न होंगे ।।
मरना है जिसको मरता, जीना है जिसको जीता।
गाती हमेशा गीता, मायूस हम न होंगे ।।
गुलशन जहाँ में कांटे, गुल खिलते रंग बिरंगे ।
हर शय में मस्त होकर, बेहोश हम न होंगे ।।
'मुक्ता' की मुक्त वाणी, बेखौफ़ होकर कहती है ।
जैसा है वैसा कहना, टस मस कभी न होंगे ।।
जिस तरह बीज का नाम ही वृक्ष, वृक्ष बीज में, बीज ही वृक्ष, बीज करके ही वृक्ष और बीज से ही वृक्ष। इसी तरह 'मैं' का ही नाम संसार 'मैं' करके ही संसार और 'मैं' ही संसारा जिस तरह मूल, शाखा, पत्ते, फूल, फल इन सबको मिलाकर वृक्ष सिद्ध होता है, इसी प्रकार सुख-दुःख, मरना-जीना, बनना-बिगड़ना इत्यादि इन सबके नाम रूप को मिलाकर ही संसार नाम पड़ा, परन्तु तारीफ तो यही है कि कौन ऐसा नाम रूप है जिसमें 'मैं' आत्मा न होऊँ, तब फिर जब 'मैं' अव्यक्त हूँ तब फिर मुझ पर कल्पित संसार भी तो, अव्यक्त ही है। इस छन्द की यही व्याख्या है, जो वेदों द्वारा स्तुति रूप में की गयी है।
यदि, इसका हृदय में स्थापना हो जाय तो व्यक्ति हमेशा के लिए शोक और मोहसे रहित हो जाय।
जिस तरह रस्सी के जल जाने के बाद भी उसका आकार-प्रकार ज्यों का त्यों बना रहता है, दीख पड़ता है, परन्तु उससे कोई चीज बाँधी नहीं जा सकती, उससे बंधन का काम नहीं हो सकता, इसी तरह ज्ञान हो जाने पर ज्ञानाग्नि से संसार प्रपंच जब जल जाता है तो वह दिखता तो वैसे ही है, उसका आकार-प्रकार तो ज्यों का त्यों बना रहता है, परन्तु वह बन्धन का कारण नहीं हो सकता।
5. राम राज्य की व्याख्या
प्रसंग है, उत्तर काण्ड के अन्तर्गत "राम राज्य वर्णन" गोरखपुरी रामायण, दोहा नं. 20वाँ के ऊपर की दो चौपाइयों से प्रारंभ होता है।
राम राज बैठे त्रैलोका । हरषित भए गए सब सोका ।
बयरु कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ।।
श्रीरामचन्द्र जी के राज सिंहासन पर बैठते ही तीनों लोक हर्षित हो गये, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता, भगवान राम के प्रताप से सबकी विषमता अर्थात् आंतरिक भेदभाव मिट गये।
दोहा- बरनाश्रम निज-निज धरम निरत बेद पथ लोग ।
चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग ।।
(उ.कां. दो. 20)
सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। देखो, राजा और प्रजा में पिता-पुत्र का संबंध होता है, जैसा पिता होगा, पुत्र भी वैसा ही होगा। इसी तरह जैसा राजा होगा, प्रजा भी वैसी ही होगी। राजा यदि धर्मात्मा है तो प्रजा भी उसी के अनुरूप होती है। जब भगवान राम सिंहासन पर बैठे तो तीनों लोक शोक और भय से रहित हो गये, क्योंकि राम भय और शोक से रहित हैं। इसलिए उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार का न भय है, न शोक है और न किसी को कोई रोग ही सताता है।
दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ।
सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ।।
राम राज में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं वेदों में तथा बतायी हुई नीति और मर्यादा में तत्पर रहकर अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं।
देखो-गौतम बुद्ध के हृदय में जब मन, वचन और कर्म से अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गयी तब जिस वन में वे तपस्या कर रहे थे वहाँ से छह मील के इर्द-गिर्द हिंसक पशुओं के हृदय में भी अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गयी, वहाँ का वायुमंडल ही ऐसा हो गया कि हिंसक पशु भी अपना स्वभाव भूल गये, सब एक घाट में पानी पीते और एक साथ प्रेम से रहते थे।
आज से सात दिन पहले यहाँ का वायुमंडल जैसा था, आज यहाँ वैसा नहीं रहा, जिस स्थल पर नित्य सात दिनों तक ब्रह्म विद्या का निरूपण हो रहा है वहाँ का परमाणु ही वैसा बन जाता है।
भगवान राम के देश में राम राज्य में अर्थात् जिसके हृदय में राम की स्थापना हो गयी वहाँ पर तापों का क्या काम? ताप तो जीव देश में रहता है, राम देश अर्थात् आत्मदेश में नहीं।
हृदय देश है, भाव सिंहासन है, इस सिंहासन पर चाहे जीव को बिठा लो, चाहे राम को। इस सिंहासन पर जब जीव बैठता है, तब इसका नाम जीवदेश हो जाता है और वहाँ पर जीव देश के विधान, कानून और धर्म लागू हो जाते हैं और जब जीव वहाँ से हट जाता है और उसमें राम बैठता है तब वहाँ राम के विधान, कानून और धर्म साथ-साथ आ जाते हैं।
'मैं' जीव हूँ, इस भाव में सारे द्वन्द्व हैं, सुख-दुःख, हर्ष-शोक, योग-वियोग, रोग-निरोग आदि वह जीव राज्य है। राम राज्य में अत्यंताभाव है, क्योंकि राम एक है दो नहीं तब वहाँ द्वंद्व कहाँ?
चारिउ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं ।
राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी ।।
धर्म के चार चरण होते हैं-सत्य, तप, दया और दान। राम राज्य में इनके चारों चरण परिपूर्ण थे। स्वप्न में भी पाप की कल्पना किसी को भी नहीं थी, सभी नर- नारी राम भक्ति और परमगति के अधिकारी थे, सब राम भक्ति में रत थे।
अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ।
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुधन लच्छन हीना ॥
सब निर्दभ धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ।
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥
राम राज्य में किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती और न किसी को कोई पीड़ा होती। सभी के शरीर सुन्दर और निरोग रहते, न कोई दरिद्र था, न दुःखी, न कोई मूर्ख था और न लक्षणहीन, सभी धर्म परायण, दम्भ रहित थे। सभी ज्ञानी और कृतज्ञ थे। वे दूसरे के किये हुए उपकार को मानने वाले थे। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं थी।
दोहा - राम राज नभगेस सुनु, सचराचर जग माहि।
काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुःख काहुहि नाहिं |21||
काल जन्य दु ख, कर्म जन्य दुःख, स्वभाव जन्य दुःख और गुण जन्य दु ख, किसी को भी राम राज्य में नहीं था।
बाल्यावस्था का दुःख बालक को नहीं, युवावस्था का दुःख युवकों को नहीं और वृद्धावस्था का दुःख वृद्धों को नहीं, ये अवस्था जन्य दुःख हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात का दुःख ये सब काल जन्य दुःख हैं। चोरी, जुआ, शराब, व्यभिचार आदि जिस कर्म के करने से दुःख मिले वह सब कर्म जन्म दुःख हैं। "इन्हें कितना भी समझाओ ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा इनका स्वभाव ही है", वह स्वभावजन्य दु ख है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जन्य जो दुःख हैं वे सब गुण जन्य दुःख हैं।
भूमि सप्त सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला ।
भुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभूता कछु बहुत न तासू ।।
सो महिमा समुझत प्रभु के री। यह बरनत हीनता घनेरी ।
सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी। फिरि एहि चरित तिन्हहुँ रति मानी ।।
सोउ जाने कर फल यह लीला। कहहिं महा मुनिबर दमसीला ।
राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकइ फनीस सारदा ।।
सब उदार सब पर उपकारी । बिप्र चरन सेवक नर नारी ।
एकनारि ब्रत रत सब झारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥
भगवान राम सारे विश्व की आत्मा हैं, जिनके एक-एक रोम में अनेकों ब्रह्माण्ड हैं उनके लिए सात द्वीपों की यह प्रभुता कोई अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे सात समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीप पृथ्वी के एकछत्र सम्राट हैं, उनकी हीनता ही है। जिनने यह महिमा जान भी ली है, उन्हें भी यह लीला बड़ी प्रिय है। इन्द्रियों का दमन करने वाले महामुनियों का ऐसा मत है। भाई! राम राज्य की सुख सम्पत्ति का वर्णन शेषजी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। राम राज्य में सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष एक पत्नीव्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियाँ भी मन, वचन और कर्म से पति सेवी और पति हितकारी हैं।
दंड जतिन्ह कर भेद जहें नर्तक नृत्य समाज ।
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचन्द्र के राज ।।22।।
श्री रामचन्द्रजी के राज्य में दण्ड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है और 'जीतो' शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनायी पड़ता है अर्थात् राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर, डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दाम, दण्ड और भेद ये चार उपाय किये जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं इसलिए 'जीतो' शब्द केवल अपने मन को जीतो के लिए ही कहा जाता है। वहाँ कोई अपराध किसी से भी नहीं होता, इसलिए दण्ड देने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं होती। अत, दण्ड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दण्ड के लिए ही प्रयोग में आता है। तात्पर्य यह कि वहाँ यदि दण्ड है तो दण्डी स्वामियों के हाथों में है, वहाँ प्रजा में नहीं है। भेद यदि है तो गाने-बजाने वालों के सुर ताल में ही है अर्थात् सुरताल के लिए 'भेद' शब्द का प्रयोग होता है और कहीं नहीं।
फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन। रहहिं एक संग गज पंचानन ।
खग मृग सहज बयरु बिसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ।।
वृक्ष, वनों में सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर वनों में एक साथ रहते हैं। पशु और पक्षी सभी स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में सब एक साथ प्रेम से रहते हैं। यह सब राजा राम की महिमा का प्रताप है।
कूजहिं खग मृग नाना बृन्दा। अभय चरहिं बन करहिं अनंदा ।
सीतल सुरभि पवन बह मंदा। गुंजत अलि लै चलि मकरंदा ।।
पक्षी मीठी बोली बोलते हैं, भाँति-भाँति के पशुओं के समूह बन में निर्भय विचरते हैं और आनन्द करते हैं। शीतल, मंद और सुगंधित पवन चलते रहता है, भौरें पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हैं।
लता बिटप मागे मधु चवहीं । मन भावतो धेनु पय सवहीं ।
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेताँ भइ कृत जुग कै करनी ॥
बेलें और वृक्ष माँगने से ही मकरन्द टपका देते हैं। गौएँ मनचाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। इसी तरह त्रेता युग में सतयुग की स्थिति आ गयी।
प्रगटीं गिरिन्ह बिबिधि मनि खानी। जगदातमा भूप जग जानी।
सरिता सकल बहहिं बर बारी। सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥
समस्त जगत् के आत्मा भगवान राम को जगत् का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रगट कर दीं, सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगीं।
सागर निज मरजादाँ रहहीं । डारहिं रत्न तटन्हि नर लहहीं ।
सर सिज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा ।।
समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात् सभी प्रदेश अत्यन्त प्रसन्न हैं।
दोहा - बिधु महि पूर मयूखन्हि, रबि तप, जेतनेहि काज ।
मागं बारिद देहिं जल, रामचन्द्र कें राज ||23||
श्री रामचन्द्र जी के राज्य में, चन्द्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से, पृथ्वी को पूर्ण कर देता है। सूर्य उतना ही तपता है जितने की आवश्यकता होती है और मेघ (बादल) माँगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही, जल देते हैं।
भाई! यह राम राज्य की महिमा का वर्णन है, जिस राम देश में, आत्म देश में, लोगों को त्रैलोक्य की विभूतियाँ भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकतीं। यह आत्म देश बड़ा ही मनोरम, शीतल, सुन्दर, अलौकिक और सन्ताप रहित है। यदि इस देश का अनुभव है तो जीव देश को तत्काल त्याग कर (क्योंकि वहाँ इसके प्रतिकूल बातें हैं) इस राम देश, आत्म देश के स्थायी निवासी बन जाओ फिर तो तुम सदा सर्वदा सारे द्वन्द्वों से मुक्त हो। यहाँ परम शांति और निर्भयता का साम्राज्य है।
6. ज्ञान-भक्ति निरुपण
आज का प्रसंग है, उत्तर काण्ड के अंतर्गत दोहा नं. 116
(ज्ञान का दीपक तथा भक्ति की महत्ता)
दोहा - यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोई।
जो जानइ रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह न होइ ॥
(उ.कां.दो. 116-क)
श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य (गुप्त मर्म) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथजी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता।
दोहा - औरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन ।
जो सुनि होइ राम पद प्रीति सदा अबिछीन ।। 116 ख।।
महात्मा कागभुशुण्डी जी, गरुड से कहते हैं कि हे सुचतुर गरुड़जी! ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिये, जिसके सुनने से श्री राम के चरणों में एक रस प्रेम होता है।
सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझत बनइ न जाइ बखानी ।
ईश्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥
मानसकार ने "अकथ कहानी" कहा है। कहानी, मनगढन्त और काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं। फिर इसे अकथ कहा, क्योंकि यह कहानी समझते तो बनती है, परन्तु कहते नहीं बनती इसलिए ही इसे अकथ कहा, यह समझने की चीज है, कहने सुनने की नहीं।
विषय समझो - जीव अविनाशी है अर्थात् सत् है, क्योंकि सत्य ही अविनाशी और अजन्मा होता है। जीव को 'अविनाशी' कहा गया, इसे अविनाशी कहते ही यह अजन्मा सिद्ध हो गया। फिर इसे 'चेतन' कहा गया, चेतन अर्थात् चित फिर 'अमल' कहा, अमल का अर्थ है विकारों से रहित अर्थात् निर्विकार और सहज सुख राशि जिसका अर्थ हुआ, स्वभावतः सुख का भण्डार है, सुख स्वरूप है, वहाँ दुःख का नामोनिशान नहीं है।
जीव के अविनाशी ने से सत्, चेतन से चित् और सहज सुख राशि से आनन्दस्वरूप हुआ अर्थात् जीव सत् है, चित् है, आनन्दस्वरूप है। इससे सिद्ध हुआ कि जीव स्वभावत, सत्, चित्, आनन्द अर्थात् 'सच्चिदानन्द' है।
तब प्रश्न होता है कि गोसाई जी ने इसे ईश्वर अंश क्यों लिखा? अरे! यही तो अकथ कहानी है, जो समझते तो बनती है, पर कहते नहीं बनती 'समुझत बनै न जाइ बखानी'।
जो पदार्थ सत्य होता है, वह एक होता है। निरवयव होता है, अखण्ड होता है, व्यापक होता है, जीव में ये सब बातें हैं, तब जीव उसका अंश कैसे हो सकता है? अरे! यही तो अकथ कहानी है, जो समझते तो बनती है, परन्तु कहते नहीं बनती और यही रघुनाथजी का रहस्य है। अब समझने के लिए विचार वाटिका में आओ- प्रश्न होता है कि जीव सगुण ईश्वर का अंश है या निर्गुण ईश्वर का अंश है? जीव को यदि सगुण ईश्वर का अंश मानो तो उसका अंश करते-करते एक दिन वह ईश्वर ही खतम हो जायेगा, क्योंकि जीववादी, जीव को अनेक मानते हैं, 'जीव अनेक एक श्रीकन्ता'। अतः, जीव सगुण ईश्वर का अंश सिद्ध नहीं होता, अब यदि जीव को निर्गुण ईश्वर का अंश कहा जाये तो निर्गुण ईश्वर अर्थात् निराकार ईश्वर का अंश नहीं हो सकता। आकाश निराकार है, फूल में गंध निराकार है, इसमें अंश-अंशी का भाव नहीं हो सकता। इस तरह जीव, निराकार ईश्वर का भी अंश सिद्ध नहीं होता, तब गोसाई जी ने अंश क्यों लिखा ? अरे! यही तो रघुनाथ जी का रहस्य है और अकथ कहानी है, जो समझते बनती है, पर कहते नहीं बनती। जीव छोटा बड़ा भी सिद्ध नहीं होता, जो समझाया जा चुका है।
निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन न जाने कोय ।
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय ।।
निर्गुण रूप सबको नित्य सुलभ है, यह सबको जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि निर्गुण रूप व्यापक आत्मा, सर्व में व्याप्त है, ओत-प्रोत है, वही व्यापक आत्मा स्वयं जो जानने वाला है और वह स्वयं ही जो नित्य 'मैं हूँ', 'मैं हूँ' बोल रहा है तो इसका अनुभव तो सब नित्य कर सकते हैं और कर रहे हैं, इसलिए निर्गुण रूप सबको सदा सुलभ है, परन्तु सगुण को समझ लेना बड़ा कठिन है, क्योंकि सगुण रूप में नाना चरित्र होते हैं और चरित्र को ही देखकर और सुनकर बड़ों-बड़ों को भी भ्रम हो जाना संभव है, जैसा कि सती को हुआ, गरुड़ को हुआ, भुशुण्डी आदि को हुआ और वे शंका में पड़ गये, जिसका परिणाम क्या हुआ? यह सब जानते हैं। इसीलिए सगुण रूप सबको सदा सुलभ नहीं है।
मानसकार ने जीव को ईश्वरका अंश कहा- इसका तात्पर्य समझो -जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, वह चेतन है अर्थात् चैतन्य है, "सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म" जानना पना उसका स्वभाव है, वह अमल अर्थात् मल रहित है, उसमें किसी प्रकार का भी मल याने विकार नहीं है, वह सहज सुखराशी है अर्थात् स्वभाव से सुख का पुञ्ज है, सुख समूह है। जीव के ये सब विशेषण हैं।
ईश्वर के जितने लक्षण और गुण है, वे सारे के सारे लक्षण जीव के हैं, जीव को ईश्वर का अंश लिखने का आशय समझो। देखो, यह एक घड़ा है, 'आकाश' अर्थात् खाली जगह या पोल इसके भीतर है। वह एक मठ या मंदिर है उसके अंदर भी वही आकाश है, इस घड़े और उस मंदिर या मठ के बाहर भी वही आकाश है, घड़े में, मट में और इनके बाहर तीनों जगह में तीन अलग-अलग आकाश नहीं है। अरे! आकाश तो एक ही है जो तीनों जगह है, घट में, मठ में और बाहर। घड़े के भीतर का आकाश, घड़े में होने के कारण घट उपाधि से घटाकाश कहलाता है, वही आकाश मठ में रहने के कारण मठ उपाधि से मठाकाश कहलाया और घट और मठ दोनों के बाहर होने से बृहदाकाश अर्थात् महदाकाश कहलाया। आकाश तो एक ही है, परन्तु भिन्न-भिन्न उपाधियों के कारण उसके अलग-अलग तीन नाम हो गये-घटाकाश, मठाकाश और महदाकाश। यदि ये उपाधियाँ हटा दी जायँ, घड़ा फोड़ दिया जाय, मठ तोड़ दिया जाय तो तीनों आकाश एक ही हो जायँ। अरे यार! इसके पहिले भी तो वह एक ही आकाश है, जो अखण्ड रूप से तीनों में ओतप्रोत है। ओत-प्रोत का अर्थ घट में आकाश, मठ में आकाश, बाहर आकाश, भीतर आकाश, ऊपर आकाश नीचे आकाश, आजू-बाजू आकाश, सब तरफ आकाश। आकाश में ही घट और मठ तथा घट और मठ में ही आकाश, चाहे उपाधि हटाओ या न हटाओ। आकाश, अखण्ड, अनन्त, अपार अविकारी, ओत-प्रोत (लबालब) पूर्ण है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक, इसी तरह वह परब्रह्म परमात्मा, अखण्ड, अनन्त, अविकारी, अपार, अगाध, लबालब पूर्ण, सर्व, आकाशवत् ओत-प्रोत है। हाँ, जैसे उपाधियों के कारण उसी एक आकाश के भिन्न-भिन्न नाम घटाकाश, मठाकाश और महदाकाश हो गये, उसी तरह भिन्न-भिन्न उपाधियों के कारण उसी एक पूर्ण अखण्ड निर्विकार शुद्ध ब्रह्म के तीन नाम हो गये। माया उपाधि से मुझ चैतन्य घनभूत आत्मा का नाम हुआ ईश्वरा अविद्या उपाधि से उसी का नाम जीव और दोनों उपाधियों से रहित जो शुद्ध चेतन है वह है ब्रह्म।
अपने आप 'मैं' आत्मा को न जानना अविद्या है, इस अविद्या उपाधि के कारण जब अपने आप 'मैं' आत्मा को कुछ माना यह है माया इस उपाधि से ईश्वर, इन दोनों उपाधियों से रहित जो है, वह है ब्रह्म।
आकाश का खण्ड नहीं हो सकता और न खण्ड किया जा सकता। वह तो अखण्ड, अनन्त और एक है। उसी प्रकार ब्रह्म का खण्ड नहीं हो सकता, उसका अंश नहीं हो सकता। वह तो अखण्ड, अपार, अनन्त सर्वत्र ओत-प्रोत है।
जगदीश ही आपसे जीव भयो, यह भी सच है वह भी सच है।
प्रतिबिम्ब कहो या बिम्ब कहो, यह भी सच है, वह भी सच है ।।
है एक नहीं यह लम्ब बयाँ, तेरी अक्ल का ही है कसूर मियाँ ।
खुर्शीद कहो या धूप कहो, यह भी सच है वह भी सच है ।।
गफ़लत से रुख का नकाब उठा, वह दम में है कसरते जल्बेनुमा ।
बुद-बुदे कहो या नीर कहो, यह भी सच है वह भी सच है ।।
है दो में एक हो दो से एक, निर्भय कर लो अन्वय-व्यतिरेक ।
अद्वैत कहो या द्वैत कहो, यह भी सच है वह भी सच है ।।
जैसे आकाश व्यापक है, अखण्ड है, उसमें अंश-अंशी भाव नहीं है, परन्तु वही आकाश घटादि उपाधि से आकाश का अंश कहलाता है। उसे हम आकाश का अंश मानते हैं, परन्तु वह वास्तविक अंश नहीं है। इसी तरह यह आत्मा आकाशवत् है और घटादिक पदार्थ क्या है? संघात। मन वाणी का जहाँ तक विषय है वह सभी संघात है।
आकाश व्यापक है, परन्तु सिर में रहने से सिराकाश, कण्ठ में रहने से कण्ठाकाश और उदर में रहने से उदराकाश उसी आकाश का नाम, इन उपाधियों के कारण पड़ जाता है। इसी तरह संघात उपाधि के कारण ही सर्व का सर्व 'मैं' आत्मा का ही नाम जीव पड़ जाता है, मगर है नहीं। अंश वही जो अंशाशी है, घटादि पदार्थों में जो आकाश, वही अशांशी। इसी तरह मुझ आत्मा का अंश, जीव, आत्मा ही है, मुझ आत्मा से जीव अलग नहीं है।
'नाम रूप दुइ ईस उपाधी ॥'
जैसे घड़ा के फूट जाने से घटाकाश, महाकाश हो जाता है। इसी तरह संघात के नाश होने से संघात में जो जीव है, वह कहीं आता-जाता नहीं, वह साक्षात् परमात्मा हो जाता है। अरे यार! परमात्मा हो क्या जाना है, परमात्मा है ही। जीव आता-जाता है, वह सब कहानी है, सैकडों लाखों वर्ष कहते-सुनते हो गये, तब भी इस जीव कहानी का अंत नहीं है, इस पर अनेक दर्शन बन गये।
निज भ्रम नहिं समुझहिं अग्यानी। प्रभु पर मोह घरहिं जड़ प्रानी।
जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ।।
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ।
उमा राम विषइक अस मोहा। नभ तम घूम घूरि जिमि सोहा ।।
(बा.कां. दो. 116 के नीचे)
वैसे लोग आकाश में अंधेरा, धुआँ और धूल आदि मानते हैं, यद्यपि ये सब उस निर्विकार शुद्ध आकाश में है नहीं, उसी प्रकार अज्ञानी जन जीव का आना-जाना, अंश-अंशी भाव मानते हैं।
तो भाई !
सो मायाबस भयउ गोसाई । बँध्यो कीर मरकट की नाई ।
जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई। जदपि मृषा छूटत कठिनई ॥
ऐसा यह जीव माया के वश होकर तोता और बंदर के समान अपने आप बिना बंधे बँधा हुआ है। इस तरह जीव चेतन और माया जड़ में ग्रंथि पड़ गयी, जो यद्यपि मृषा है अर्थात् गाँठ पड़ी नहीं है, पर बंध गया है। इससे छूटना बड़ा कठिन है।
इस पर एक दृष्टांत सुनो-जिस जंगल में बहुत से तोते रहते हैं तोता पकड़ने वाला बहेलिया वहाँ जाता है और उस झाड़ पर जिसमें कि तोते रहते हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर एक पतली लम्बी रस्सी अरगनी जैसे बाँध देता है, फिर उसमें छोटी- छोटी, पतली-पतली बहुत-सी पोंगरियाँ गूँथ देता है। (पोंगरियाँ, पंखों में लगी पोंगरी जैसे होती है, जिससे पंखा घूमता है।) इसके बाद उन पोंगरियों में तोतों के खाने के कुछ पदार्थ चिपका देता है। यह सब करके वह बहेलिया पास ही ओट में कहीं जा बैठता है और वह फँसने पर पकड़ने के लिए तोतों की प्रतीक्षा करता रहता है। तोते, भोजन की लालच में आकर उन पोंगरियों में बैठते हैं, उनके वजन से पोंगरियाँ घूम जाती हैं और उस पर बैठे हुए तोते पोंगरी को पकड़े हुए उल्टे लटक जाते हैं। तोते समझते हैं कि अरे! पोंगरी ने हमें पकड़ लिया। अब हम इससे किसी तरह नहीं छूट सकते। वे पोंगरी को पकड़े हुए उल्टे लटके रहते हैं।
इतने में एक दयालु सज्जन उसी तरफ से निकल पड़े, उन्हें तोतों की दशा देखकर उन पर बड़ी दया आयी। वे उनके पास गये और उनसे पूछने लगे कि भाई, यह क्या बात है? तुम सब इस तरह क्यों उल्टे लटके पड़े हो।
तब तोतों ने उत्तर दिया, क्या करें महाराज। हम सब दाना चुगने यहाँ आये थे कि इन पोंगरियों ने हम सबको पकड़ लिया, वे छोड़ती ही नहीं और हम सब यहाँ से छुटकारा ही नहीं पा सक रहे हैं। तब उस दयालु महात्मा ने उन्हें उससे छूटने के लिए उपदेश दिया और कहा-ऐ तोते! तुम सब चैतन्य हो, पोंगरी जड़ है वह तुम्हें कैसे पकड़ सकती है। तुम स्वयं पोंगरी को पकडे हो। अतः, तुम सब पोंगरी को छोड़ दो और इसी क्षण उड़ जाओ। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम सबके सब मुक्त हो ऐसा उपदेश देकर महात्मा चले गये।
वे सब तोते पोंगरी को पकड़े हुए उल्टा लटके, इस उपदेश का बार-बार पाठ करने लगे, रटने लगे, वे सब कहते जाते थे कि ऐ तोते! तुम सब चैतन्य हो, पौंगरी जड़ है, वह तुम्हें कैसे पकड़ सकती है, तुम स्वयं पोंगरी को पकड़े हो। अतः, तुम सब पोंगरी को छोड़ दो और इसी क्षण उड़ जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम सबके सब मुक्त हो। वे सब तोते ऐसा कहते तो जाते थे, परन्तु पोंगरी कोई नहीं छोडता था।
महात्मा ने उन्हें यह उपदेश, पाठ करने के लिए बार-बार रटने के लिए नहीं दिया था बल्कि उसके अनुसार कार्य करने के लिए दिया था। यदि वे तोते उस उपदेश का भाव समझकर उसके अनुसार कार्य करते तो तुरन्त सब उड़ सकते थे, परन्तु अज्ञानी तोतों को इतना ज्ञान कहाँ ? उल्टा लटके-लटके सभी तोते इस उपदेश का पाठ कर ही रहे थे कि इतने में बहेलिया आया और जैसे झाड़ से फल तोड़-तोड़ कर कोई अपने थैले में डालता जाता है, इस तरह बड़े आराम से सब तोतों को पोंगरी से उठा-उठाकर अपने पिंजड़े में डालता गया और अंत में अपने घर की राह ली।
इन तोतों के ही समान, बंदरों की भी दशा होती है। बंदर पकड़ने वाले लोग छोटी-छोटी सुराही, जिसका मुँह सँकरा होता है जमीन में पास-पास गाड़ देते हैं और उनमें बंदरों के खाने के पदार्थ चने आदि रख देते हैं। बंदर आता है और अपने चंचल स्वभाव के अनुसार बड़ी चपलता से उसे देख लेता है, फिर वह इस सुराही मे चने निकालने के लिए अपना हाथ डालता है और चने से मुट्ठी को भर लेता है, चने से भरी हुई मुट्ठी बाहर निकालने के लिए बंदर बार-बार उसे अपनी ओर खींचता है परन्तु चने से भरी हुई मुट्ठी सुराही का मुँह छोटा होने के कारण बाहर निकल नहीं सकती, वह सुराही के भीतर अटक जाती है। वह मुट्टी से चने छोड़ दे तो मुट्टी सहज ही बाहर निकल जाय, परन्तु वह मुट्ठी से चने छोड़ता भी नहीं और अपनी मुट्ठी बाहर निकाल भी नहीं सकता। वह समझता है कि बस सुराही ने मुझे पकड़ लिया है अब इससे छूटना मुश्किल है। देखो बंदर चेतन है और सुराही जड़। भला जड़ सुराही चेतन बंदर को क्या पकड़ सकती है, बंदर स्वयं उसे पकड़ा हुआ है। वह वहीं सुराही में हाथ डाले बैठा रह जाता है कि बंदर पकड़ने वाला आता है और आसानी से उसे पकड़कर बाँध लेता है।
भाई! यह है दृष्टान्त, इसका द्राष्टांत यह है कि मनुष्य कहता है कि हम क्या करें भाई "माया के चक्कर में पड़े हैं" इससे छूटना कठिन है, उनके ऐसा कहने का तात्पर्य यह कि माया के चक्कर में वे खुद ही अपने आप पड़े हैं, माया ने इन्हें चक्कर में नहीं डाला। प्रश्न होता है कि किसने कहा कि तुम माया के चक्कर में पड़ो। उत्तर होगा-किसी ने नहीं, वे स्वयं पड़े हैं। वेदशास्त्र सन्त, महात्मा जन इन्हें उपदेश करते हैं कि भाई! माया जड़ है, तुम चैतन्य हो, माया तुम्हें क्या पकड़ सकती है, माया को तुम पकड़े हो, माया को तुम छोड़ दो, फिर तो इसी क्षण तुम मुक्त हो।
लोग उनके द्वारा दिये गये उपदेशों के अनुसार काम नहीं करते। वे उन उपदेशों के भाव को समझकर वैसा व्यवहार नहीं करते, बल्कि प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि करके, चन्दन, तिलक लगाकर आसन जमाकर बैठते हैं और बड़ी श्रद्धा से इन उपदेशों का नित्य पाठ करते हैं। बार-बार रटते हैं और इस तरह पाठ करके तोतों की नाई वे बन्धन से मुक्त होना चाहते हैं। इससे बन्धन से छुटकारा तो मिलता नहीं, मृत्यु रूपी बहेलिया आता है और उन्हें आराम से तोतों की नाई उठा ले जाता है। ये जन्म जन्मांतर भी इसी तरह उपेदेशों, वेद शास्त्रों का पाठ करते रहें तो बन्धन से मुक्त नहीं हो सकते। यदि उन उपदेशों के अर्थ और भाव को समझकर उनके अनुसार कार्य और व्यवहार करें तो वे उसी क्षण मुक्त हैं। इस पर एक दूसरा दृष्टांत सुनो -
एक बार किसी नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। उनकी दयालुता, मृदुभाषिता और आकर्षक प्रवचन का लोगों के हृदय में ऐसा प्रभाव पड़ा कि रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे तथा वहाँ नित्य आनन्द की वर्षा होने लगी।
उनका उपदेश सुनने के लिए उस नगर का बनिया भी नित्य जाया करता था। वह प्रवचन समाप्त होने के बाद जब अपने घर आता, तब अपने घर के लोगों को भी स्वामीजी के उपदेश का हाल बताया करता था। उस बनिये के घर में एक तोता पला था, वह तोता भी यह हाल बनिये से बड़े ध्यान से सुना करता था।
एक दिन नियत समय पर जब वह बनिया, स्वामीजी के प्रवचन में जाने के लिए तैयार होकर चलने लगा, तब पिंजरे में बंद तोते ने बनिये से कहा भाई! आप स्वामीजी का उपदेश नित्य सुनकर आनन्दित होते हैं, आज मेरी ओर से भी महात्मा जी से प्रार्थना कीजिये और उनसे कहिये कि वे मुझे भी कुछ उपदेश देने की दया करें। बनिये ने तोते की बातें सुनी और कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मैं स्वामी जी को सुना दूंगा। यह कहते हुए बनिया प्रवचन सुनने चला गया।
स्वामी जी का प्रवचन समाप्त होने के बाद बनिया ने तोते की प्रार्थना स्वामीजी को सुनायी और कहने लगा कि महाराज! पिंजड़े में बन्द तोते ने बड़ी नम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना की है और कहा है कि मेरे लिए स्वामीजी का क्या उपदेश है? पूछकर आना।
तोते का संदेश सुनते ही महात्मा अपने आसन पर बैठे ही बैठे मूर्च्छित होकर गिर पड़े, उनकी आँखें फिर गयी, हाथ पैर छटपटाने लगे और चेहरे का रंग उड़ गया। महात्मा की ऐसी दशा देख लोग चारों ओर दौड़ पड़े, कोई भीड़ हटाने लगा, किसी ने पंखा किया कोई पानी छिड़कने लगा और किसी ने तेल की मालिश की। इस तरह बड़ी तत्परता से उनका उपचार किया गया, बड़ी देर बाद बड़ी कठिनाई से स्वामीजी को होश में लाया जा सका।
लोग बनिये को डाँटने लगे और उससे कहने लगे कि तुमने ऐसा क्या अशुभ और बुरा संदेश स्वामी जी को सुनाया जिसके कारण स्वामीजी की ऐसी दशा हुई। बनिया यह सब डॉट-फटकार सुनकर चुपचाप अपने घर चला गया। घर पहुँचने पर तोते ने बड़ी आशा भरे नेत्रों से बनिये की ओर देखा और उससे पूछने लगा 'भाई! आपने मेरी प्रार्थना स्वामीजी को सुनाया?
तोते की बात सुनते ही बनिया बड़े क्रोध में आ गया और वहाँ की घटना का सब विवरण तोते को सुनाकर कहने लगा कि तूने कैसा अशुभ संदेश भेजा था कि जिसे सुनते ही स्वामीजी की ऐसी दशा हुई और लोगों के द्वारा मुझे भी खरी-खोटी सुननी पड़ी।
बनिये के द्वारा वहाँ की घटना का हाल सुनते ही तोता पिंजड़े के भीतर ही बड़े जोर से फड़फड़ाया और मूर्च्छित होकर गिर पड़ा, वह बेहोश हो गया, उसकी आँखें पथरा गयीं और पैर ऊपर टँग गये। यह दुखद समाचार सुनते ही पडोस के बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गये।
इस घटना को देखते ही बनिया बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, भगवन्! यह क्या रहस्य है कि तोते की भी महात्मा जैसी दशा हो गयी। बनिये ने तोते को तुरन्त ही पिंजड़े से बाहर निकाला और उसे पानी आदि छिड़कने का प्रबन्ध करने लगा।
तोता पिंजड़े से बाहर होते ही तुरन्त उड़कर आँगन के झाड़ पर दूर जा बैठा और कहने लगा-नित्य भगवत कथा सुनने वाले प्रेमीजनों! भव सागर से पार होने तथा माया के बन्धन से छूटने के लिए वेदशास्त्र, रामायण, गीता तथा उपनिषद् आदि का उपदेश, स्वामीजी के श्रीमुख से नित्य सुन रहे हो, परन्तु केवल सुनना ही सुनना है, उसके अर्थ और भाव को समझकर वैसा ही कार्य और व्यवहार करना नहीं है। उन उपदेशों को आचरण में नहीं उतारना है, तब बन्धन से छुटकारा कैसे हो सकता है। देखो, मेरा संदेश सुनकर दयालु महात्मा ने मुझे कैसा उपदेश दिया, वे मूर्च्छित होकर आसन पर गिर पड़े, बेहोश हो गये और मृतवत् दिखने लगे। इसका अर्थ था कि बेटा! तू भी इसी तरह आचरण करना, तुझे मुक्ति मिल जायगी।
मैंने उनके द्वारा दिये गये उपदेश का अर्थ समझा और उसे अपने आचरण में लाया, परिणाम तुम्हारी आँखों के सामने है। मैं तुरन्त बंधन से मुक्ति पा गया। अतः, वेद शास्त्र और सन्त-महात्माओं के उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं हैं वरन् उन्हें आचरण में लाने के लिए हैं तभी उसका फल प्राप्त हो सकता है।
अब आ जाओ प्रसंग पर, अंश वही जो अंशाशी है, घटाकाश अंश है, अंशांशी आकाश है। अंश, अंशाशी है। देखो, लकड़ी का अंश लकड़ी ही होगा मिट्टी या पत्थर नहीं। सोना का अंश सोना ही होगा, ईंट-पत्थर नहीं। लोहे का अंश करोगे तो लोहा ही होगा, मिट्टी या लकड़ी नहीं। इसी तरह ईश्वर का अंश ईश्वर ही है, जीव नहीं।
'है' यह अस्तित्व जो है, वह भगवान आत्मा ही है। 'देह है' अब इस 'है अस्तित्व को ही देह मान लिया, देह मान्यता तो जड़ है, अभाव रूप है, विकल्प है, और 'है' अस्तित्व चेतन है, भगवान आत्मा है। इन दोनों में अर्थात् मान्यता देह जड़ और 'है' अस्तित्व चेतन आत्मा इन दोनों में ग्रंथि है जो बडी सुगमता से पडती है। (देह मान लेना क्या कोई कठिन है) परन्तु बडी कठिनाई से छूटती है, यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या है।
जो माना जाय वह जड़ है और जिसको माना जाय वह चेतन है। आधार और आधेय, जब दोनों मिल गये तो यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। इसी को 'चिज्जड़ ग्रंथि' भी कहते हैं। जो स्वरूप को ढाँके वह मूल अविद्या है और जो पदार्थ को ढाँके वह तूल अविद्या है। अपने स्वरूप का अज्ञान मूल अविद्या है, ज्ञान से मूल अविद्या का नाश होता है।
तब ते जीव भयउ संसारी । छूट न ग्रन्थि न होइ सुखारी ।
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक-अधिक अरुझाई ।।
जीव हृदय तम मोह बिसेषी । ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी ।
अस संजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ।।
इस मिथ्या ग्रंथि के पड़ने से जीव संसारी हो गया। अब न तो गाँठ छूटती है और न वह सुखी होता है। यद्यपि वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय छूटने के बताये हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन् अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय इस गाँठ को देख ही नहीं सकता, तब खोले कैसे? जब कभी ईश्वर की कृपा से ऐसा संयोग आ जाता है, तब कहीं कदाचित् वह ग्रंथि छूट पाती है। आत्म जिज्ञासा ही ईश्वरकृत संयोग है।
अपना आप जब दिखे, तब ग्रंथि दिखाई दे, मगर अज्ञान अंधकार के कारण न तो अपना आप ही दीख पडता है और न ग्रंथि ही। रामायण पढते-पढते जिंदगी बीत रही है मगर ग्रंथि छूटी नहीं बल्कि नित्य उलझती चली जा रही है। जब ईश्वरकृत संयोग हो अर्थात् आत्म जिज्ञासा जागे कि 'मैं' कौन हूँ? इसको जानने के लिए हृदय में मछली के समान तड़प हो। अरे! यही तो ईश्वरकृत संयोग है और क्या ईश्वर पेड़ पर बैठा है जो आकर बतायेगा, जब मैं स्वयं ही तोता और बन्दर की तरह बंधा हूँ, तब मैं स्वयं ही उस बंधन को खोलूंगा, दूसरा कौन खोलेगा? जैसे, कोई स्वयं कमरे के भीतर, भीतर से सँकल लगाकर पड़ा हो और कहता हो अरे भाई! मुझे बाहर निकालो, मेरा बन्धन खोलो तो उसे कौन दूसरा बाहर निकाल सकता है, जब दूसरा बाँधा हो, तब वह खोले और जब स्वयं ही बन्धन लगाया है, तब वह स्वयं ही खोलेगा। अब आगे ज्ञान दीपक का प्रसंग आता है- यहाँ से साधन शुरू होता है।
सात्त्विक श्रद्धा घेनु सुहाई। जौं हरि कृपाँ हृदयें बस आई ।
जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ।।
भगवान की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुन्दर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाय। असंख्यों जप, तप, व्रत, यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार (आचरण) जो श्रुतियों ने कहे हैं -
तेइ तृन हरित चरै जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ।
नोइ निवृत्ति पात्र बिस्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा ।।
उन्हीं धर्माचार रूपी हरी घास को जब वह गौ चरै और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पेन्हावे। सांसारिक विषयों से और प्रपंच से मन का हटना यही गौ को दुहते समय पिछले पैर बाँधने की रस्सी अर्थात् नोई है, विश्वास दूध दुहने का पात्र है, बरतन है। निर्मल, निष्पाप मन जो है, जो अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है।
परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटै अनल अकाम बनाई ।
तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावै । घृति सम जावनु देइ जमावै ॥
मुदिताँ मथै विचार मथानी । दम अधार रजु सत्य सुबानी ।
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता । बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ।।
इस प्रकार परम धर्म मय दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली- भाँति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठण्डा करे और धैर्य तथा शम (मन का निग्रह) रूपी जामन देकर उसे जमावे, फिर प्रसन्नता रूपी कमोरी में सत्व विचार रूपी मथानी से दम (इन्द्रिय दमन) के आधार पर (दम रुपी खम्भे आदि के सहारे) सत्य और सुन्दर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर उसमें से निर्मल, सुन्दर और अत्यन्त पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें।
दोहा - जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ ।
बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ ।।117 क।।
फिर योग रूपी अग्नि प्रगट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे और सब कर्मों को योग रूपी अग्नि से भस्म कर दे और जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल-जल जाय तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठण्डा करे।
तब बिग्यानरुपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ ।
चित्त दिआ भरि धरै दृढ़ समता दिअटि बनाइ ।।117 ख।।
तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दीये को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढतापूर्वक जमाकर रखे।
दोहा - तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काढ़ि ।
तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करै सुगादि ।।117 ग।।
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएँ और सत, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रुई को निकाल कर और फिर उसे सँवार कर उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान मय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे आदि जल जायँ।
अब दीप जल गया।
सोहमस्मि इति वृत्ति अखण्डा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ।
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा ।।
'सोहमस्मि' वह ब्रह्म 'मैं' हूँ, यह जो अखण्ड तैल धारावत् कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुन्दर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल, भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है।
प्रबल अबिद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटइ अपारा ।
तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा। उर गृहुँ बैठि ग्रन्थि निरुआरा ।।
अब महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट गया, तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर मे बैठकर ग्रंथि को खोलती है।
अब यहाँ पर शंका होती है कि जब दीपक जल गया, उजाला हो गया, आत्मानुभूति हो गयी, अविद्या का परिवार नष्ट हो गया तो फिर अब वह कौन-सी ग्रंथि रह गयी है, बच रही है, जिस ग्रंथि को बुद्धि हृदयदेश में ज्ञान के प्रकाश में खोलने बैठती है।
भैय्या! वेद शास्त्रों के बड़े-बड़े ज्ञाता तथा विद्वान भी इसका भाव नहीं लगा पाते। यह बड़ा जटिल प्रश्न है। इसका अनुभव तो अनुभवी संत ही करता है और जिस पर संत कृपा हो चुकी है और अनुभव जगत् में जिसका अधिकार है वही इसका भाव लगा पाता है।
छोरन ग्रंथि पाव जौं सोई। तब यह जीव कृतारथ होई ।
छोरत ग्रंथि जानि खगराया। विघ्न अनेक करइ तब माया ।।
यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गाँठ को खोल ले, तब यह जीव कृतार्थ हो जाय, कागभुसुण्डी जी कहते हैं कि हे पक्षिराज गरुड़ जी। गाँठ खोलते हुए जानकर फिर माया अनेकों विघ्न करती है। भाई! अब यहाँ पर माया विघ्न करने दौड़ती है, प्रश्न होता है कि माया का क्या बिगड़ता है, जो विघ्न करने दौड़ती है।
इसका कारण सुनो - जब तुम अपने आपको कुछ भी मानते हो, देह, स्त्री, पुरुष, जीव आदि अथवा चाहे ब्रह्म भी मानते हो तब तक माया तुम्हारा प्रेरक है, पति है, स्वामी है और जब अपने आपको जैसा का तैसा, जहाँ का वहाँ, जो का सो जाना कि 'मैं' तो शुद्ध तत्त्व भगवान आत्मा हूँ। न मैं बद्ध था, न मुक्त हुआ। न अज्ञानी था और अब ज्ञानी हुआ। न मैं जीव था, अब ब्रह्म हुआ। इसी का नाम बोध है।
जैसे थे वैसे रहे, अब कछु कहा न जाय ।।
मानसकार के शब्दों में इसी को "परम प्रकाश" कहा है। इस स्थिति में फिर तुम माया के पति हो गये। माया के तुम प्रेरक, स्वामी हो गये, फिर तो जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है, उसी प्रकार तुम माया को नचा सकते हो।
जब माया देखती है कि अब यह मेरा पति होने जा रहा है, फिर तो मुझे इसके वश में रहना पड़ेगा, ऐसा समझकर ही वह विघ्न करने दौड़ती है। वह तुम्हें अपना पति (माया पति) नहीं होने देना चाहती।
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई ।
कल बल छल करि जाहिं समीपा। अंचल बात बुझावहिं दीपा ।।
माया बहुत सी ऋद्धि-सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे ऋद्धि-सिद्धियाँ अपनी कला से, बल से और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। जब मैं ब्रह्म हूँ, तब दूसरों के हृदय की बात को क्यों नहीं जान लेता, पानी क्यों नहीं बरसा लेता, पानी बरसना बंद क्यों नहीं कर सकता, नदी में पूर में पानी के ऊपर चलकर उस पार क्यों नहीं चला जाता, मेरे सभी संकल्प पूरे क्यों नहीं होते आदि मन में इस तरह के अनेक विघ्नों का जाल बिछ जाना, वही माया की प्रेरणा में रिद्धि-सिद्धियों द्वारा बुद्धि को लोभ दिखाना है।
होइ बुद्धि जौं परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी।
जौं तेहि बिघ्न बुद्धि नहीं बाधी । तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी ।।
यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन ऋद्धि-सिद्धियों को हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती तक नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तब फिर देवताओं का उपद्रव शुरु होता है।
इन्द्री द्वारा झरोखा नाना। तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना ।
आवत देखहिं विषय बयारी । ते हठि देहिं कपाट उघारी ।।
इन्द्रियों के द्वार हृदय रूप घर में अनेकों झरोखे हैं वहाँ प्रत्येक झरोखे में देवता अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं।
जब सो प्रभंजन उर गृहुँ जाई। तबहिं दीप बिग्यान बुझाई ।
ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि बिकल भइ विषय बतासा ।।
ज्यों ही वह तेज हवा, हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गाँठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गयी, सारा किया कराया चौपट हो गया।
इन्द्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई ।
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ।।
इन इन्द्रियों के देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति है इसलिए ही वे ज्ञान का विरोध करते हैं और वे बड़े-बड़े उपद्रव करते हैं। कारण यह है कि अज्ञानी जीव-देवताओं के पशु हैं, उनके द्वारा जो पूजा-पाठ, यज्ञ-हवन आदि किये जाते हैं वे सब देवताओं को ही मिलते हैं। यही उनका भोग है। इन अज्ञानी जीवों के बल पर ही उनका निर्वाह होता है। ऐसे ये देवता जब देखते हैं कि अरे! यह तो ज्ञानोपार्जन में लग रहा है, इसको यदि स्वरूप का बोध हो गया, तब इससे पूजा-पाठ, हवन आदि सब छूट जायेगा, हमको यह नहीं पूजेगा, हम अभी तक इसे अपना पशु बनाये थे, अब यह हमसे छूटकर भागना चाहता है, तब जिस तरह घोड़े या गधे के मालिक का घोडा या गधा जिस पर कि वह बोझा लादकर अपना व्यवसाय चलाकर निर्वाह करता है, खूँटे से छूटकर भाग जाये और उनका बोझा लादना बंद हो जाये, तब उस मालिक को जैसे महान दुःख होता है, उसी तरह ये अज्ञानी जीव जो देवाताओं के पशु हैं और जन्म-जन्मांतर से उनका बोझा ढो रहे हैं, उन्हें जब वे अपने चंगुल से छूटकर भागते देखते हैं (स्वरूप का बोध हो जाना ही देवताओं के बंधन से छूटना है) तब इन देवताओं को बड़ा दुःख होता है। इन देवताओं की पशुओं की रक्षा उनके एजेंट लोग करते हैं, ये कमीशन एजेंट वे हैं जो इन अज्ञानी जीवों को उपदेश देते हैं कि भाई! देओगे तब पाओगे, उस जन्म में दिये थे तो इस जन्म में पा रहे हो, दान, जप, तप, होम करोगे तो स्वर्ग जाओगे और वहाँ अनेक प्रकार के सुख भोगोगे। इनकी बातों पर विचार करो, देखो इन स्वर्ग जाने वालों में से आज दिन तक अपने परिवार के लोगों के नाम ऐसा कोई पत्र नहीं आया कि बेटो! तुम लोग हमारी चिंता न करना, हमें यहाँ "एयर कंडीशन" की कोटी मिली है, हम यहाँ सब प्रकार से सुखी हैं, तुम घर का सब सार सम्भाल बड़े ध्यान से करते रहो, उनके द्वारा न तो ऐसा पत्र ही आया और न उनमें से कोई आकर ही बताया कि स्वर्ग में हमें इस तरह की सुख, सुविधा मिली थी। बस, मान लो स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक की कल्पना अज्ञानियों के लिए है, ये केवल कहानी है और कहानी बच्चे सुना करते हैं। वास्तव में न कहीं स्वर्ग है और न नरक, स्वर्ग और नरक सब यहीं है।
भाई! इस तरह के उपदेश देने वाले, उपदेशक भेदवादी गुरु घंटाल ही देवताओं के कमीशन एजेंट हैं। इन्हें चाहे तेली कह लो, मतलब एक ही है। छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत से तेली सत्संगी हैं, परन्तु इन तेलियों के विषय में नहीं कहा जा रहा है, अरे भाई! ये तेली हैं भी नहीं। तेली तो वे हैं, जिन्हें ज्ञान से विरोध है। तेली बैलों को कोल्हू में जोतते हैं, उन बैलों की आँखों में टोपा बाँध देते हैं, जिससे उन्हें कुछ दिखाई न दे, वे बैल दिन-रात कोल्हू में चलते हैं। वे बीस-बीस, तीस-तीस मील चल चुकते हैं, परन्तु रहते हैं अपनी ही जगह, वहीं के वहीं। अगर बैल थकावट के मारे कहीं खड़ा होता है तो तेली उसे तुतारी (बैल हाँकने का डण्डा जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली कील लगी होती है) से हुदरथय (कोंचता है) तब वह बैल फिर सिर हिलाते हुए चलने लगता है।
भाई! संसार कोल्हू है, अज्ञानी जीव बैल है, इन्हें उपदेश देने वाले जो भेदवादी गुरु घंटाल हैं, वे तेली हैं, जीव बैलों की आँखों में अज्ञान का टोपा बँधा है, पुण्य-पाप कर्म रूप, तिल, अलसी, मूंगफली आदि तिलहन हैं, जिन्हें पेरकर तेल निकाला जाता है, इनसे सुख-दुःख रूपी तेल, घल-घल, घल-घल निकल रहा है। कर्त्ता, भोक्ता का अहंकार धानी है। अब थकावट के मारे बैल के खड़े होने का मतलब यह है कि यदि वह अज्ञानी जीव कभी भूले-भटके किसी सन्त-महात्मा के सत्संग में चला जाता है और उनका उपदेश सुनने लगता है और यह बात उनके भेदवादी गुरु घंटाल अथवा उपदेशक (तेली) जान लेता है, तब वह उसे वाणी रूप तुतारी से कोंचता है, हुदरता है। वह उसे धमका कर कहता है अरे! तू कहाँ चला गया था, तुझे ज्ञान में अधिकार नहीं है, ज्ञान तो संन्यासियों की चीज है, जब तक घर-द्वार छोड़कर बाबा न बन जायगा, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। तुझसे पूजा-पाठ, करम-धरम सब छूट जायगा और तू नास्तिक हो जायगा, फिर तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आज गया तो गया, खबरदार! अब भविष्य में वहाँ कभी न जाना। इनके द्वारा ऐसा धमकाना ही हुदरना है, तब वह अज्ञानी जीव बैल सिर हिलाते हुए पुनः उनके बताये मार्ग पर चलने लगता है। यही देवताओं के विघ्न करने का तात्पर्य है।
अब आ जाओ प्रसंग पर बुद्धि को विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, तब फिर उस बुझे हुए ज्ञान दीपक को दुबारा कौन जलावै।
दोहा - तब फिरि जीव बिबिध बिधि पावइ संसृति क्लेस ।
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस || 118-क।।
इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति अर्थात् जन्म-मरणादि के क्लेश पाता है, भाई ! भगवान की माया अत्यन्त दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। बस ! ज्ञान दीपक का यहीं पर उपसंहार है।
अब प्रश्न होता है कि अहं ब्रह्मास्मि 'मैं' ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान साधन से प्राप्त किया या अपने आप? उत्तर होगा-साधन से। तब फिर साधन का फल नित्य नहीं होता, वह अनित्य होता है। साधन से दीप जला था। अतः, वह बुझेगा ही। अब वह कौन- सी ग्रंथि है, जिसे बुद्धि हृदय देश में ज्ञान के प्रकाश में खोलने बैठती है? उत्तर सुनो- आज के पहिले मैं जीव था, आज ब्रह्म हुआ। अगर आज मैं साधन से ब्रह्म हुआ हूँ तो कल फिर जीव हो सकता हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, इसमें 'मैं' और 'ब्रह्म' ये दो की झलक जो है, उनमें 'मैं' कौन और 'ब्रह्म' कौन? बस, यही ग्रंथि है जिसे बुद्धि ज्ञान के प्रकाश में खोलने बैठती है। प्रश्न होता है, वह खोलने वाली बुद्धि कौन-सी है? उत्तर है- फिर वही 'सुमति कुदारी' अर्थात् ब्रह्माकार रूपी बुद्धि है, जिससे खोजना है। यद्यपि मानसकार ने उस ग्रंथि का उल्लेख नहीं किया है। जब ज्ञान हुआ तब मैं ब्रह्म हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, मैं साक्षी हूँ आदि भावना की गयी। प्रश्न है किस पर? उत्तर है 'मैं' पर। इसीलिए यह भावनात्मक ज्ञान हुआ। पहिले 'मैं' पर देह भाव था, फिर 'मैं' पर जीव भाव और अब 'मैं' पर ब्रह्म भाव आया। ये तीनों भाव तीन गुण हैं जो 'मैं' पर आरोपित हैं। अब विचार करना है कि जागृत अवस्था में भले ही ब्रह्म भाव रहे, स्वप्न अवस्था में भी मान लो ब्रह्म भाव रहे, परन्तु गाढी नींद, सुषुप्ति अवस्था में इस भाव का सर्वथा अभाव हो जाता है, यदि ब्रह्म भाव सत्य होता तो सुषुप्ति अवस्था में भी उसका अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य त्रिकाला बाध्य होता है। इससे सिद्ध होता है कि जैसे देह भाव अनित्य, जीव भाव अनित्य, उसी प्रकार यह ब्रह्म भाव भी अनित्य ही हुआ।
प्रश्न होता है कि जिस ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, वह ज्ञान सत्य है या असत्य? यदि, उस ज्ञान को सत्य कहो तो एक तो ब्रह्म सत्य और दूसरा वह ज्ञान सत्य इस तरह दो सत्य हो गये तब सत्य तो एक ही है, सत्य दो नहीं हो सकते। इसमें वेदान्त का द्वैतापत्ति दोष आता है। तब यह सिद्ध हुआ कि वह ज्ञान असत्य है।
अब फिर प्रश्न होता है कि असत्य से सत्य का ज्ञान कैसे होगा? जब यह ज्ञान असत्य है, तब उसके द्वारा जो ज्ञान हुआ वह भी असत्य ही है। तो इसका प्रमाण स्वप्न के शेर को स्वप्न की गोली से मारे जाने का है। जैसे, किसी ने स्वप्न में जंगल में कोई शेर देखा तब उस स्वप्न के शेर को वह जागृत अवस्था की गोली से मारेगा अथवा स्वप्न अवस्था की गोली से मारेगा? उत्तर होगा- स्वप्न अवस्था की गोली से मारेगा। तब स्वप्न का शेर असत्य और स्वप्न की गोली असत्य, इस तरह असत्य से असत्य का निवारण होता है। इसी तरह भावनात्मक ज्ञान 'अहं ब्रह्मस्मि' मैं ब्रह्म हूँ भी असत्य और जिस ज्ञान से उसे जाना वह ज्ञान भी असत्य। तब जाना किसको? किसी को नहीं। क्या पाया? कुछ भी नहीं। जैसा पहिले था, वही अब हूँ, वैसा ही आगे रहूँगा। न मैं पहिले अज्ञानी था और अब ज्ञानी हुआ, न मैं पहिले बद्ध था और अब मुक्त हुआ, न मैं पहिले जीव था और अब ब्रह्म हुआ। यही अविद्या की ग्रंथि है, जो खोली जाती है। जिस तरह पैर में काँटा गड़ जाने पर उसे दूसरे काँटे से निकाला जाता है और जब पैर का गड़ा हुआ काँटा निकल जाता है, तब वहनिकला हुआ काँटा और जिस काँटे से वह काँटा निकाला गया वह काँटा, ये दोनों काँटे साथ-साथ फेंक दिये जाते हैं, उसी प्रकार अनादि काल से हृदय में अज्ञान रूपी काँटा गड़ा था, देह मानना, स्त्री, पुरुष मानना, जीव मानना आदि इस अज्ञान रूपी काँटे को 'अहंब्रह्मास्मि' रूपी काँटे से निकाला जाता है और फिर दोनों काँटे साथ-साथ फेंक दिये जाते हैं।
मैं ब्रह्म हूँ, इसका प्रमाद होता है 'मैं' हूँ, इसका प्रमाद नहीं होता। 'अहंब्रह्मास्मि' के निकल जाने पर जो शेष रह जाता है, वही विशुद्ध तत्त्व 'मैं' हूँ जहाँ परम शांति है।
यदि 'मैं' न होऊँ तो ब्रह्म की धारणा किस पर करोगे? जितनी भी धारणाएँ हैं- देह धारणा, जीव धारणा, ब्रह्म धारणा ये सब धारणाएँ 'मैं' पर ही किया जाता है। सर्व धारणाओं के बाध हो जाने के बाद जो शेष रह जाये वह 'मैं' आत्मा ही नित्य हूँ, कालातीत हूँ, भगवान हूँ, जो निर्विरोध सर्व मान्य सिद्धान्त है। 'मैं' हूँ, वह सर्व का अपना आप है, यहीं पर जीव कृतकृत्य होता है।
'अहंब्रह्मास्मि' ज्ञान दीपक है, इसके लिए तो दीया चाहिये, घी चाहिये, तब यह जलता है, परन्तु 'मैं' हूँ, इसके लिए भी क्या इन सब सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है? नहीं। 'मैं' आत्मा तो परम प्रकाश हूँ, सहज प्रकाश हूँ, स्वाभाविक प्रकाश हूँ।
परम प्रकास रूप दिन राती। नहीं कछु चहिअ दिआ घृत बाती ।
राम भगति चिन्तामनि सुन्दर । बसइ गरुड़ जाके उर अंतर ।।
गरल सुधासम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ।
राम भगति मनि उर बस जाके । दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके ।।
चतुर सिरोमनि तेइ जगमाहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ।
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई। राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई ।।
सुगम उपाय पाइने केरे । नर हत भाग्य देहिं भटभेरे ।
पावन पर्वत बेद पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना ।।
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी । ग्यान बिराग नयन उरगारी ।
भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुखखानी ।।
मोरें मन प्रभु अस बिस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ।
राम सिंधु धन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि सन्त समीरा ॥
सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु सन्त न काहूँ पाई ।
अस बिचारि जो कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा ।।
दोहा- ब्रह्म पयोनिधि मन्दर ग्यान सन्त सुर आहिं ।
कथा सुधा मथि काढ़हिं भगति मधुरता जाहिं ।। 120 क।।
बिरति चर्म असि ग्यान, मद लोभ मोह रिपु मारि ।
जय पाइअ सो हरि भगति, देखु खगेस विचारि ॥ 120 ख।।
भैय्या! भक्ति की ऐसी महिमा है। इसे चाहे भक्ति कह लो 'मैं' पद कह लो, आत्मा कह लो या भगवान कह लो, सबका एक ही मतलब है। 'मैं' को मणि की उपमा दी गयी 'मैं' आत्मा सर्व का ज्ञाता हूँ, ज्ञान को जानता हूँ, अज्ञान को जानता हूँ, सूक्ष्म को जानता हूँ, स्थूल को जानता हूँ, 'मैं' क्या नहीं जानता? बस, यही नारायण पद है, भगवत पद है और यहीं पर पूर्ण विश्रान्ति है।
श्री मानसकार ने आत्म पद न कहकर भक्ति पद कहा है, क्योंकि जिस समय रामायण की रचना हुई उस समय का देश-काल वैसा ही था। 'मैं' पद स्वतंत्र है इसके अधीन ज्ञान और विज्ञान है।
सो सुतंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ।।
'मैं' ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का आधार 'मैं' यह ज्ञान है। 'मैं' सर्व हूँ, सर्व का आधार 'मैं', यह विज्ञान है। इस तरह ज्ञान और विज्ञान का 'मैं' ही आधार हुआ। 'मैं' यह भक्ति है।
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ।।
आत्म पद स्वतंत्र है, परन्तु बिना सतसंग के (संतों के संग के) यह दुर्लभ है। यह तो सन्त शरण से ही, सन्त समागम से ही प्राप्त होता है। यद्यपि 'मैं' हूँ, यह अनुभव सबको है, परन्तु यह ज्ञान सबको कहाँ है कि 'यह अनुभव सबको है।' क्या यह भी अनुभव है कि यह ज्ञान सबको है? बस, इसी ज्ञान का सन्त महात्मा जन अनुभव कराते हैं। भक्ति सब गुणों की खानि है, जो गुण देखना चाहो, इसमें देख लो, 'मैं' को देह देख लो, स्त्री देख लो, पुरुष देख लो, जीव देख लो, ब्रह्म देख लो, पशु-पक्षी, कीट, पतंग, जो भी देख लो वह उसी रूप में दिखता है, क्योंकि मैं आत्मा सर्व में, सर्व रूप से, सर्व होकर, सर्व का सब कुछ होकर उसमें जो हूँ, जो सकलगुण खानी ही तो हुआ। इसीलिए तो इसे चिंतामणि की उपमा दी गयी। चिंतामणि को जिस रूप में देखना चाहो, वह उसी रूप में दिखाई देता है। यह अनुभव, अनुभव होते हुए भी, बिना सन्त शरण के अनुभव नहीं होता। दीपक के नीचे तो अंधेरा रहता है, परन्तु क्या सूर्य के नीचे भी अंधेरा रहता है? नहीं। 'मैं' आत्मा सर्व का प्रकाशक हूँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्था और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल, सबको जानता हूँ, परन्तु 'मैं' सब कुछ जानता हूँ यह कहाँ जानता हूँ। परन्तु 'मैं' सबका अनुभव करता हूँ, परन्तु 'मैं' सबका अनुभव करता हूँ, यह कहाँ जानता हूँ। बस, इसी के लिए सन्त शरण की जरूरत पड़ती है।
सन्त विशुद्ध मिलहिं परितेही । चितवहिं राम कृपा करि जेही ।
जिन सन्तों की कृपा से भक्ति चिन्तामणि प्राप्त होती है, वे सन्त कब मिलते हैं? अरे। जब भगवान की कृपा होती है, तब सन्त मिलते हैं और जब सन्त की कृपा होती है, तब भगवान मिलते हैं, एक पहलू के दो नाम चाहे सन्त कहो या भगवाना नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि ऐसी जो भक्ति है, वह कब प्राप्त होती है? तो वे कहते हैं कि -
महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्व ||38||
अर्थात् महान पुरुषों की कृपा से और भगवान की कृपा से यह भक्ति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि महात्माओं का संग और उनका मिलना तो बडा दुर्लभ है -
महत्संगस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ||39||
अर्थात् जिन सन्तों की कृपा से यह भक्ति मिलती है, उनका मिलना तो बड़ा दुर्लभ है, वे कब मिलते हैं? तो वे कहते हैं कि -
लभ्यते ऽपि तत्कृ पयैव ।।40।।
अर्थात् जब भगवान की कृपा होती है, तब ऐसे सन्त मिलते हैं। जिन सन्त की कृपा से भगवान मिलते हैं, उन सन्त के प्रति क्या भाव होना चाहिए? तो कहते हैं कि-
तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात् ।।41।।
उन सन्त में और भगवान में भेद का अभाव है। रे! दोनों एक ही हैं। उन संत के प्रति हृदय में नारायण भाव होना चाहिए, क्योंकि नर से तो कल्याण नहीं होता, कल्याण तो नारायण से ही होता है। उनके प्रति भगवत भाव, नारायण भाव आये बिना स्वरूप भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यदि साधन करना ही है तो सन्त मिलने का साधन करो, सन्तों को साधो । सन्त साधन साध्य है, भगवान कृपा साध्य है।
भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो सन्त होईं अनुकूला ।।
इसलिए भाई! सन्त मिले और अनुकूल हो जायें तभी सर्व सुखों का मूल जो अनुपम भक्ति है, वह मिलती है।
प्रश्न होता है सन्तों की अनुकूलता क्या है? अरे ! उनके प्रति नर भाव न होकर नारायण भाव हो जायें, वे नारायण के रूप में दिखने लगें तो समझ लो कि सन्त अनुकूल हो गये। यही सन्त की अनुकूलता है।
मैं तो उन सन्तों का दास, जिन्होंने मन मार लिया।
मन मारा, तन वश में कीन्हा, भरम भयो सब दूर ॥
बाहर से कछु दीखे नाहीं, अन्दर बरसै नूर ।
जिन्हों ने मार मन लिया
आपा मारि जगत से बैठे, नहीं किसी से काम ।
उनमें तो कछु अंतर नाहीं, सन्त कहो चाहे राम ।।
जिन्हों ने मन मार लिया ।।2।।
नरसिंह जी के सद्गुरु स्वामी, वह रस दिया पिलाय ।
एक बूंद सागर में मिल गयो, क्या करेगा यमराज ।।
जिन्हों ने मन मार लिया ।।3।।
मैं तो उन सन्तों का दास, जिन्होंने मन मार लिया ।।
बस! यहीं पर "ज्ञान भक्ति निरूपण' प्रसंग का उपसंहार है।
7. भगवान शंकर और माता पार्वती सम्वाद
अब अंतिम प्रसंग है भगवान शंकर और माता पार्वती सम्वाद भगवान शंकर के श्रीमुख द्वारा, माता पार्वती जब समरत रामायण सुन चुकीं, तब वह विनम्र भाव से भगवान शंकर से कहती हैं -
प्रसंग है गोरखपुरी रामायण उत्तरकाण्ड रामायण दोहा नं. 52 (क)
दोहा- तुम्हरी कृपाँ कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह ।
जानेउँ राम प्रताप प्रभु चिदानन्द सन्दोह ।।52-क।।
नाथ तवानन ससि सवत कथा सुधा रघुबीर ।
श्रवन पुटन्हि मन पानकरि नहीं अघात मतिधीर 1152-ख।।
माता जी कहती हैं- हे कृपा सागर! आपकी कृपा से अब मैं भगवान राम का जो वास्तविक स्वरूप है, उसे समझ गयी और उनके प्रताप और महिमा को जान गयी। हे नाथ! आपके चन्द्रमा रूपी मुख कमल से, जो कथामृत निकल रहा है उसे मैं अपने दोनों कानों से पी रही हूँ, परन्तु तृप्ति नहीं हो रही है, अभी उसकी प्यास बनी हुई है, क्योंकि
राम चरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ।
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरि गुन सुनहिं निरंतर तेऊ ॥
यदि कोई कहता है कि राम कथा सुनकर मैं अब तृप्त हो गया तो समझ लो कि उसने अभी कथा के महत्त्व और भगवान विश्वात्मा की महिमा को नहीं जाना, जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी निरन्तर भगवान के गुण और महिमा को सुनते हुए कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि "हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता" जब हरि और उनकी कथा दोनों अनन्त हैं, तब तृप्ति कैसी?
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रति पाद्य राम भगवाना ।।
वस्तुतः, राम कथा तो वही है, जिसके आदि, अन्त और मध्य में भगवान श्रीराम विश्वात्मा का जो चराचर के अस्तित्व हैं उनकी और उनके चरित्र की व्याख्या हो, नहीं तो वह राम कथा नहीं, केवल किस्सा कहानी है।
भव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कहें दृढ़ नावा ।
विषइन्ह कहें पुनि हरि गुन ग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ।।
जो संसार सागर से तरना चाहते हैं, उसके लिए भगवान श्रीराम की कथा नौका के समान है। भगवान का गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनन्द देने वाले हैं।
श्रवनवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ।
ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ।। जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, उसे आत्मघाती कहते हैं। प्रश्न होता है कि आत्मा तो अजर, अमर, नित्य है, तब इसका घात कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर है-देखो, मानसकार कहते हैं कि -
नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ।
करनधार सद्गुरुदृढ़ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ।।
दोहा- जो न तरै भव सागर, नर समाज अस पाइ ।
सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाइ ॥
(उ.कां. दो. 44)
देखो, नदी पार करने के लिए इतनी सामग्री की जरूरत होती है केंवट, नाव, अनुकूल वायु और पतवार। सद्गुरु जो है वह केंवट है। मनुष्य शरीर यह नाव है। भगवान की कृपा जिसके कारण मानव शरीर मिला यही अनुकूल वायु है तथा श्रद्धा और विश्वास यही पतवार है। इस तरह इन सामग्रियों को पाकर भी जो भवसागर नहीं तरता, वही आत्मघाती अर्थात् आत्म हत्यारा है।
ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥
मानसकार ने जीव को यहाँ पर जड़ कहा, इससे मालूम होता है कि चेतन जीव भी होता है, तो भाई! जिसने अपने आपको संसारी जीव माना है वही जड़ जीव है और जिसने अपने आपको आत्मा अनुभव किया है वही चेतन जीव है।
हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा ।
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुसुंडी गरुड़ प्रति गाई ॥
दोहा- बिरति ग्यान बिग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह ।
बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ||52||
माता जी विनयपूर्वक पूछती हैं कि हे नाथ! आपने श्रीराम चरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैं अपार सुखी हुई। आपने जो कहा कि यह सुन्दर कथा कागभुसुण्डी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौए का शरीर पाकर भी कागभुसुण्डी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं और उनका श्रीराम जी के चरणों में अत्यन्त प्रेम है, फिर उन्हें श्रीराम 'रघुनाथ' जी की भक्ति भी प्राप्त है, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है, क्योंकि हे नाथ!
नर सहस्त्र महें सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म ब्रतधारी ।
धर्मसील कोटिक महें कोई । बिषय बिमुख बिराग रत होई ।।
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ग्यान सकृत कोउ लहई।
ग्यानवंत कोटिक महें कोऊ । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥
तिन्ह सहस्त्र महुँ सब सुख खानी । दुर्लभ ब्रह्म लीन बिज्ञानी ।
धर्मसील बिरक्त अरु ग्यानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ।।
सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ।
सो हरिभगति काग किमि पाई। बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥
राम परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर ।
नाथ कहहु कारन, पायउ काक सरीर ।।54।।
हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मात्मा होता है। इन करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, जो धर्म करे उसे धर्मात्मा कहते हैं। जिस कार्य के करने में लज्जा और भय न हो वह कर्म 'धर्म' कहलाता है और जिस कर्म के करने में हृदय में लज्जा और भय हो वही 'अधर्म' है। धर्म करने से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध अन्तःकरण में ही वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्यवान को ही भगवान को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। ऐसे करोड़ों विरक्तों में से कोई एक भगवान को सम्यक प्रकार से जानता है। जीव भी अपने आप को जानता है, परन्तु वह 'मैं' अमुक हूँ ऐसा जानता है, यह जानना केवल जानना है, यह सम्यक् प्रकार से जानना नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि -
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकोमामजमव्ययम् ।।7/25।।
योग माया करके 'मैं' आत्मा ढँका हुआ हूँ, इसलिए सब मुझे नहीं जान पाते। दो के जोड़ को योग कहते हैं, जड़ और चेतन दोनों के मेल को योग कहते हैं। 'मैं जीव हूँ', इसमें 'मैं' हुआ चेतन और जीव हुआ जड़, इन दोनों के मेल को योग कहते हैं। मैं जीव हूँ, इसमें 'मैं' हुआ चेतन और 'जीव' हुआ जड़ इन दोनों का जोड है, 'मैं जीव हूँ' यह हुआ योग और मानने का नाम माया है। योग और माया दोनों मिलकर हो गया 'योग माया' इसी में 'मैं' आत्मा ढका हुआ हूँ, इसीलिए सब मुझे जान नहीं पाते। जानते तो हैं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जीव हूँ, मैं अमूक हूँ आदि, परन्तु यह सम्यक् प्रकार से जानना नहीं है 'मैं' का 'मैं' ही हूँ, इस प्रकार का जानना ही सम्यक् प्रकार से जानना है।
प्रश्न होता है कि ढक्कन कैसे उघारा जाये और कौन उघारेगा? उत्तर है- अरे! जब दूसरा कोई ढक्कन लगाया हो तो दूसरा उघारे और जब स्वयं ही ढक्कन लगाया है तब स्वयं ही उघारेगा। सन्त महात्मा जन तो केवल उपदेश देते हैं, जब अपने आपको जाना, अनुभव किया तो यही तो ढक्कन का उघरना है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक प्रकार से मुझे जानता है, ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक जीवन मुक्त होता है अर्थात् जीते जी मुक्त होता है। ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खानि ब्रह्म में लीन, विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवनमुक्त और ब्रह्मलीन इन सबमें भी माताजी कहती हैं कि हे नाथ! वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है, जिसके मद और माया नष्ट हो गये हों और जो राम भक्ति में रत हों। हे प्रभु! ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया? मुझे इसका रहस्य समझाकर कहिये, यह जानने की मेरी बड़ी जिज्ञासा है।
सबते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ।।
सबसे परे की वह कौन-सी भक्ति है, जिसे पाकर मद और माया, दोनों गत अर्थात् नष्ट हो जाते हैं। भाई ! उस भक्ति का स्वरूप सुनो-
मान्यता का नाम माया है। मान्यताभिमान का नाम मद और अनुभूति का नाम रत् है। तीनों के आधार का नाम भक्ति है।
लकड़ी को डण्डा मान लेना मान्यता (माया) और डण्डा मैं हूँ समझना मद अर्थात् अभिमान और लकड़ी की अनुभूति होना अर्थात् अपने आप डण्डे का लकड़ी अनुभव करना यह हुआ रत और तीनों का आधार जो लकड़ी है यह हुआ भक्ति।
जो भी विकल्प किया जाता है उसका कोई न कोई आधार होता है। इसी प्रकार यदि आत्मा न हो तो देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन सबका विकल्प किस पर होगा? सोने पर आभूषण का, मिट्टी पर घड़े का, सूत पर वस्त्र का और लकड़ी पर डण्डे का विकल्प हुआ। इन विकल्पों को ढूँढने चलो तो विकल्प मिलते नहीं केवल आधार ही हाथ लगता है। इसी प्रकार मुझ भगवान आत्मा पर सारे चराचर का विकल्प है। जैसे, लकड़ी को माना डण्डा, इसी प्रकार मुझ आत्मा को माना संसार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि। अपने 'मैं' को माना देह यह हुआ मान्यता अर्थात् माया और देह मानकर फिर समझा कि में देह हूँ यह हुआ अभिमान और जब अपने 'मैं' को जाना कि 'मैं' आत्मा हूँ तो यह हुआ रत और इसमें निष्ठा हो जाना यही भक्ति है।
माता पार्वती पूछती है कि हे प्रभु! ऐसे श्रीराम परायण, ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुसुण्डी जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया और आपने इसे किस प्रकार सुना, यह सब जानने का मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। कृपाकर मुझे यह सब सुनाइये।
गरुड़ महाग्यानी गुन रासी । हरि सेवक अति निकट निवासी ।
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ।।
कहहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा ।
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई ।।
हे नाथ! गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, भगवान के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले, उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौए के पास जाकर रामकथा किस कारण सुनी और फिर इन दोनों हरि भक्तों का किस तरह सत्संग हुआ, सो कहिये।
पार्वती जी की सुन्दर और सरल वाणी को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वे आदर के साथ बोले -
धन्य सती पावन मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ।
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा ।।
उपजइ राम चरन बिस्वासा । भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा ।
हे सती! तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा प्रगाढ़ प्रेम है। अब तुम उस परम पवित्र इतिहास को सुनो, जिसके सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्रीराम के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है।
दोहा- ऐसिअ प्रस्न बिहंग पति कीन्हि काग सन जाइ ।
सो अब सादर कहिहउँ सुनहु उमा मन लाइ ||55||
पक्षिराज गरुड़ ने भी कागभुसुण्डी से जाकर ऐसे ही प्रश्न किया था। हे उमा ! मैं वह सब कथा आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो -
पूर्व जन्म में जब तुम सती के रूप में थी, तब तुम्हारे पिता दक्ष ने हमारा अपमान किया। उस अपमान को तुम न सह सकीं और यज्ञ में जाकर तुम जल मरी, तुम्हारे वियोग के दु ख से मैं व्याकुल हो इधर-उधर घूमने लगा। घूमते-घूमते मैं भुसुण्डी के आश्रम में गया, वहाँ नित्य हरि कथा होती है और दूर-दूर से बड़े-बड़े अनेक पक्षी उस कथा में सम्मिलित होते हैं। मैं भी हंस का रूप धारण कर वहाँ गया, क्योंकि पक्षियों में पक्षी रूप में ही शामिल होना उचित था। वहाँ मैं बहुत दिनों तक सत्संग में रहा और उनके द्वारा भगवान राम के पवित्र चरित्र और महिमा को सुनकर फिर कैलाश लौट आया।
हे गिरिजा! अब वह कथा सुनो, जिस कारण से गरुड़ जी कागभुसुण्डी के पास गये थे।
जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रीड़ा। समुझत चरित होति मोहिं ब्रीड़ा।
इन्द्रजीत कर आपु बँधायो। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो ।
बन्धन काटि गयो उरगादा। उपजा हृदयँ प्रचण्ड बिषादा ।
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती । करत बिचार उरग आराती ॥
ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । माया मोह पार परमीसा ।
सो अवतार सुनेऊँ जग माही। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥
दोहा - भव बंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम ।
खर्ब निसाचर बाँधेउ नाग पास सोइ राम ।।58।।
जब रघुनाथ जी ने रणक्रीड़ा किया (वास्तविक क्रीड़ा नहीं) वह यह कि जब राम-रावण का युद्ध हो रहा था, उस लीला को याद करके अभी भी लज्जा आती है। भगवान राम इन्द्रजीत मेघनाथ के हाथ से नागफाँस में आप बंध गये। उन्हें बाँधा नहीं गया, वे स्वयं बंध गये, अपने आप बंधाए, फिर क्या था, कोलाहल मच गया कि भगवान को इन्द्रजीत ने बांध लिया, तब नारद ने गरुड़ को बन्धन काटने के लिए भेजा, क्योंकि गरुड़ उरगारि हैं, सर्पों के शत्रु हैं। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी ने बन्धन को क्षण मात्र में काट दिया तब उनके हृदय में बहुत प्रकार से विषाद और विचार उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे कि जो व्यापक ब्रह्म हैं, सर्व का सर्व हैं, विरज हैं अर्थात् जिनका शरीर रज वीर्य से पैदा नहीं हुआ और जो माया, मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, जगत् में उन्हीं का अवतार हुआ है ऐसा मैंने सुना था, परन्तु देखा कुछ और ही। यदि, मैं अभी नहीं आता तो वे अभी बन्धन में ही पड़े रहते। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बन्धन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागफाँस में बाँध लिया उनमें कुछ प्रताप न रहा, कैसा आश्चर्य है, क्या ये वही राम हैं? बस, गरुड बाबा चक्कर में पड़ गये और चकनाचूर हो गये।
भैय्या! अधिष्ठान में भ्रम हो जाना महान दुःख का कारण होता है। भगवान शंकर कहते हैं- हे पार्वती! गरुड को उसी प्रकार का भ्रम हुआ, जिस प्रकार तुमको हुआ था।
नाना भाँति मनहिं समुझावा । प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा ।
खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई । भयउ मोहबस तुम्हरिहिं नाई ।।
ब्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं। कहेसि जो संसय निज मन माहीं।
सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनुखग प्रबल राम के माया ।।
गरुड़ ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया पर उन्हें शांति न मिली, तब वे व्याकुल होकर देवर्षि नारद के पास गये और अपनी सब व्यथा उन्हें सुनायी। उसे सुनकर नारदजी को दया आ गयी। उन्होंने कहा- हे गरुड जी! भगवान राम की माया बड़ी ही बलवती है।
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई। बरिआई बिमोह मन करई ।
जेहिं बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ।।
महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें ।
चतुरानन पहिं जाहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ।।
जो ज्ञानियों के चित्त को हरण कर लेती है और उन्हें भ्रम में डाल देती है। हे भाई! इस माया ने मुझको भी अनेक बार नचाया है। आपके हृदय में महा मोह उत्पन्न हो गया है यह मेरे समझाने से तुरन्त नहीं मिटेगा। इसलिए हे भाई! आप ब्रह्माजी के पास जाइये और वे जैसा कहें वैसा ही कीजिये।
दोहा- अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान ।
हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ।।59।।
ऐसा कह नारद जी तुरन्त वहाँ से चल पड़े, वे डर गये कि देखने की अपेक्षा सुनने से अधिक भ्रम पैदा होता है, यह संक्रामक रोग है। अत, इससे वे बचना चाहते थे, क्योंकि वे भोग चुके थे।
तब खगपति बिरंचि पहिं गयऊ। निज संदेह सुनावत भयऊ ।
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ।।
मन महुँ करइ बिचार बिधाता । मायाबस कबि कोबिद ग्याता ।
हरि माया कर अमिति प्रभावा। बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ।।
यह पक्षिराज गरुड़जी ब्रह्माजी के पास गये और अपनी सारी कथा उन्हें कह सुनायी, जिसे सुनकर ब्रह्माजी सोचने लगे कि अरे! कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव अपार है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है।
अग जगमय जग मम उपराजा । नहि आचरज मोह खगराजा ।
तब बोले बिधि गिरा सुहाई। जान महेस राम प्रभुताई ॥
बैनतेय संकर पहिं जाहू । तात अनत पूछहु जनि काहू ।
तहँ होइहि तव संसय हानी । चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी ।।
ब्रह्मा सोचने लगे कि यह सारा जगत् मेरा रचा हुआ है, जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब औरों को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसा सोच वे गरुड़ जी से प्रेम से बोले कि हे तात! भगवान शंकर, श्रीराम की महिमा को भली- भाँति जानते हैं तुम उनके पास जाओ, परन्तु भाई! एक बात ध्यान में रखना, वह यह कि उनसे केवल अपने काम की ही बात कहना, अन्य कुछ नहीं कहना, नहीं तो अकड़बम्ब बाबा हैं, कुछ का कुछ हो जाना संभव है। ब्रह्माजी के इस वचन को सुनकर कि वहीं तुम्हारी सब शंकाएँ दूर होंगी, गरुड़जी भगवान शंकर के पास चल पड़े।
भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती! तब बड़ी आकुलता से, आतुरतावश, गरुड़ मेरे पास आये। उस समय मैं कुबेर के घर निमंत्रण में जा रहा था और तुम कैलाश में थी।
दोहा- परमातुर बिहंगपति, आयेउ तब मों पास ।
जात रहेउँ कुबेर गृह, रहिहु उमा कैलास !160||
गरुड़ ने आकर आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और मुझको अपना संदेह सुनाया। उनकी विनती और कोमल वाणी को सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा कि-
मिलेहु गरुड़ मारग महँ मोही। कवन भाँति समझावौं तोही ।
तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा ।।॥
हे भाई! अभी मैं कुबेर के यहाँ जा रहा हूँ और तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस तरह समझाऊँ, सब शंकाओं का तो तभी नाश होगा जब बहुत समय तक सत्संग किया जाये।
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ।
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ।।
नित हरि कथा होत जहें भाई। पठवउँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ।
जाइहि सुनत सकल संदेहा । राम चरन होइहि अति नेहा ।।
उस सत्संग में सुन्दर हरि कथा सुनी जाये जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है। राम कथा उसी को कहते हैं, जिसके आदि, अन्त और मध्य में राम की ही व्याख्या हो। हे भाई! जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है मैं तुमको वहीं भेजता हूँ। तुम वहाँ जाकर उसे सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जायेगा और भगवान के चरणों में तुम्हारा अत्यन्त प्रेम होगा। देखो - यहाँ पर भगवान शंकर ने गरुड को कोई साधन नहीं बताया कि जाओ, योगाभ्यास करो, उल्टा-सीधा टंगो, एक पैर से खड़े रहो आदि। उन्होंने केवल सन्त महान पुरुषों के सत्संग को ही साधन बताया, जिससे भ्रम और मोह का निवारण होता है।
दोहा- बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग।
मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ||61||
बिना सत्संग के हरि कथा सुनने को नहीं मिलती और बिना हरि कथा के सुने मोह का नाश नहीं होता और बिना मोह के नाश हुए भगवान श्रीराम के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता।
भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा! मैंने गरुड़ से, कागभुशुण्डी के आश्रम और उसकी महिमा का गान किया और उन्हें उनके पास ही भेजा, क्योंकि दोनों पक्षी जाति के ही थे। अतः एक-दूसरे के दोनों अनुकूल थे। हे भवानी! प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है, जिसे वह न मोह ले। मैंने काग भुशुण्डी के संबंध में गरुड से कहा -
मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा। किएँ जोग तप ग्यान बिरागा ।
उत्तर दिसि सुन्दर गिरि नीला। तहँ रह कागभुसुंडी सुसीला ॥
राम भगति पथ परम प्रबीना । ग्यानी गुन गृह बहु कालीना ।
राम कथा सो कहइ निरन्तर । सादर सुनहिं बिबिध बिहंगबर ।।
जाइ सुनहु तहैं हरि गुन भूरी । होइहि मोह जनित दुख दूरी ।
मैं जब तेहि सब कहा बुझाई। चलेउ हरणि मम पद सिरु नाई ।।
ताते उमा न मैं समुझावा । रघुपति कृपाँ मरमु मैं पावा ।
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवै चह कृपानिधाना ।।
कछु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा । समुझइ खग खगही के भाषा ।
प्रभु माया बलवंत भवानी। जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥
दोहा- ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान।
ताहि मोह माया नर पावर करहिं गुमान 1162 क।।
जो गरुड़ ज्ञानियों और भक्तों में शिरोमणि हैं और जो स्वयं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी जब माया ने मोह लिया तब फिर नीच मनुष्य कैसे मूर्खतावश अभिमान करते हैं।
दोहा- सिव बिरंचि कहुँ मोहइ को है बपुरा आन ।
अस जियें जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान ।।62 ख।।
यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब अन्य बेचारों की क्या गिनती? ऐसा मन में विचार कर मुनि जन भगवान का निरन्तर भजन करते रहते हैं। शिवजी कहते हैं कि हे गिरिजा ! मेरे इस सुझाव को मानकर गरुड़, कागभुशुण्डी के आश्रम में गये और वहाँ जाकर उसने बहुत दिनों तक सत्संग किया, जिससे उसके शोक और मोह का नाश हुआ और फिर उन्हें शांति मिली।
दोहा- गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन ।
बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं वेद पुरान ।। 125 ख।।
हे गिरिजा! सन्त समागम के समान विश्व में दूसरा कोई लाभ नहीं, परन्तु वह सन्त समागम बिना हरि की कृपा के हो नहीं सकता, ऐसा वेद और पुरान गाते हैं।
कहेउँ परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छूटहिं भव पासा ।
प्रनत कल्पतरु करुना पुंजा । उपजइ प्रीति राम पद कंजा ॥
मन क्रम बचन जनित अघ जाई। सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई।
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग बिराग ग्यान निपुनाई ।
नाना कर्म धर्म ब्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥
भूत दया द्विज गुरु सेवकाई । बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई ।
जहँ लगि साधन बेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी।
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपा काहूँ एक पाई ॥
हे भवानी! वेदों ने जहाँ तक साधन बताया है, उन सबका फल, श्री हरि की भक्ति ही है, किन्तु श्रुतियों में गायी हुई वह श्रीराम जी की भक्ति राम की ही कृपा से, कोई एक बिरला ही पाता है।
मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास ।
जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिस्वास ।।62-क।।
जो मनुष्य विश्वासपूर्वक निरन्तर यह कथा सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं।
सोइ सर्बग्य गुनी सोई ग्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ।
धर्म परायन सोइ कुल त्राता । राम चरन जाकर मन राता ।।
नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धान्त नीक तेहिं जाना ।
सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाँड़ि भजइ रघुबीरा ।।
धन्य देस सो जहँ सुरसरी । धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी ।
धन्य सो भूपु नीति जो करई। घन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ।
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ।।
जिनका मन श्रीराम के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, पण्डित है, दानी है, धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धान्त को भली-भाँति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है।
वह देश धन्य है जहाँ गंगा बहती है। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से कभी नहीं डिगता। वह धन धन्य है, जिसकी पहली गति होती है। धन की तीन गतियाँ होती हैं दान, भोग और नाश।
धन रे मारग तीन कहे हैं, दान भोग औ नास ।
दिया और खाया नहीं जाता, वह धन होय विनास ।।
वह बुद्धि धन्य और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी धन्य है, जब सत्संग हो और वह जन्म धन्य है, जिसमें ब्राह्मण की अखण्ड भक्ति हो।
दोहा- सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत ।
श्रीरघुबीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत ||127||
हे उमा! सुनो-वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुबीर परायण, अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। उस विनम्र पुरुष की माला की कोख शुद्ध हो जाती है, वह देश पवित्र हो जाता है और उससे पृथ्वी पवित्र हो जाती है।
मति अनुरूप कथा मैं भाषी । जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ।
तव मन प्रीति देखि अधिकाई । तब मैं रघुपति कथा सुनाई ।।
यह न कहिअ सठही हठ सीलहि। जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि ।
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि। जो न भजइ सचराचर स्वामिहि ॥
द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहुँ । सुरपति सरिस होय नृप जबहूँ ।
राम कथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह कें सत संगति अति प्यारी ॥
गुर पद प्रीति नीति रत जेई । द्विज सेवक अधिकारी तेई ।
ता कहें यह बिसेष सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्री रघुराई ।।
मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसे छिपाकर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथजी की यह कथा तुमको सुनायी।
यह कथा उनसे न कहनी चाहिए, जो धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी, और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते उनसे यह कथा नहीं कहना चाहिए।
ब्राह्मणों के द्रोही यदि वह देवराज इन्द्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हों, तब भी यह कथा उन्हें नहीं सुनाना चाहिए। श्रीराम की कथा के अधिकारी तो वे ही हैं, जिन्हें सत्संगति अत्यन्त प्रिय है। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं और उनको ही यह कथा बहुत सुख देने वाली है, जिनको श्री रघुनाथजी प्राण के समान प्यारे हैं।
दोहा - राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्बान ।
भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान || 128||
जो श्रीराम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष चाहता हो तो वह उस कथा रूपी अमृत को प्रेमपूर्वक अपने कान रूपी दोने से पीयें।
राम कथा गिरिजा मैं बरनी। कलिमल समनि मनोमल हरनी।
संसृति रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावहिं श्रुति सुरी ॥
एहि महें रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना ।
अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देइ एहि मारग सोई ।।
भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजा! मैंने कलियुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया, यह राम कथा जन्म-मरण रूपी रोग के नाश करने के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें सात सुन्दर सीढियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यन्त कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है।
मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ।
कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं ।।
जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं, जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गी के खुर से बने हुए गड्ढे के जल की भाँति पार कर जाते हैं।
सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजां बोली गिरा सुहाई ।
नाथ कृपाँ मम गत संदेहा । राम चरन उपजेउ नव नेहा ॥
भगवान राम की यह कथा सुनकर माता पार्वती अत्यंत हर्षित हुई और वे सुन्दर वाणी में बोली कि हे नाथ! आपकी कृपा से मेरा सब संदेह जाता रहा और भगवान राम के चरणों में नवीन और दृढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ।
दोहा- मैं कृतकृत्य भइउँ अब तव प्रसाद बिस्वेस ।
उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस ||129||
हे विश्वनाथ! आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गयी, मुझमें दृढ राम भक्ति उत्पन्न हो गयी और मेरे सम्पूर्ण क्लेश बीत गये।
भाई! भगवान शंकर और माता पार्वती का यह संवाद सभी संशय भ्रम और शोक-मोह को नाश कर सम्पूर्ण प्रकार के सुख और शांति का देने वाला है। अस्तु, अंत में -
राम अमित गुन सागर, थाह कि पावइ कोइ ।
सन्तन्ह सन जस कछु सुनेउँ, तुमहिं सुनायेउँ सोइ ॥
ॐ शांतिः ! शान्तिः! शांतिः !!!