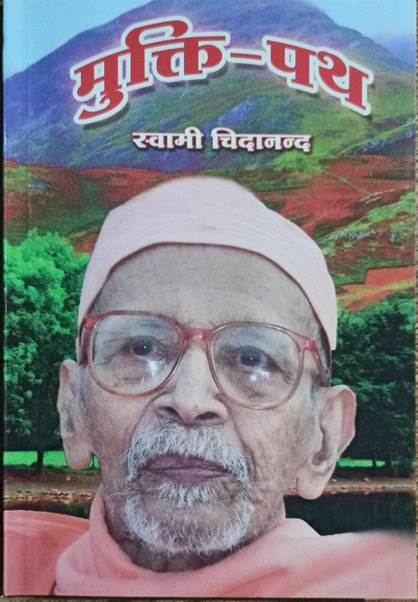
मुक्ति-पथ
PATH TO BLESSEDNESS
का हिन्दी अनुवाद
स्वामी चिदानन्द
अनुवादिका
श्रीमती गुलशन सचदेव
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९ १९२
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण : १९७६
द्वितीय हिन्दी संस्करण : १९९१
तृतीय हिन्दी संस्करण :२०१७
(५०० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
HC 24
Price: 70/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए
स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त
फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर-२४९ १९२,
जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित।
For online orders and Catalogue visit: disbooks.org
आमुख
ॐ शान्तिः ! त्रिविध ताप शान्त हो ।
'मुक्ति-पथ' नामक यह पुस्तक आत्म-संयम, मनोनिग्रह, एकाग्रता एवं ध्यान के द्वारा अन्तरात्मा के साक्षात्कार का सरल निरूपण है। भारत के महान् ऋषि तथा आचार्य महर्षि पतंजलि लगभग पाँच सहस्र वर्ष पूर्व मानवता के कल्याण हेतु योग-विज्ञान का सार लघु, संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण सूत्रों के रूप में छोड़ गये। प्रस्तुत पुस्तक उनके लोक-विश्रुत इन सूत्रों पर आधारित है। अत्यन्त संक्षिप्त तथा सारगर्भित होने के कारण इन सूत्रों का अर्थ एक बार के अध्ययन से समझना कठिन है। इन सूत्रों की व्याख्या की आवश्यकता थी। अठारह पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने पातंजल योग-सूत्रों का भाष्य लिख कर हमारे लिए यह कार्य किया। प्रचुर समयोपरान्त एक विद्वान् शिष्य एवं साधक वाचस्पति मिश्र ने महर्षि व्यास के भाष्य पर एक विस्तृत अर्थद्योतक टीका लिखी। प्रस्तुत पुस्तक के पाठ उपर्लिखित योग-शास्त्र पर आधारित हैं।
मैंने इन पाठों को क्यों लिखा ? इनको लिखने का प्रयोजन क्या था ? यह सम्पूर्ण पुस्तक आध्यात्मिक मार्ग के जिज्ञासु साधकों की सेवा तथा एक ऐसे महत् ज्ञान के प्रचार व प्रसार का हार्दिक प्रयास है जो मानव-जाति के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आज से अनेक वर्ष पूर्व अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी की स्पष्ट इच्छा एवं आदेशानुसार मैंने यह कार्य सहर्ष आरम्भ किया। उन्होंने इस बीसवीं सदी के साधकों की सेवा के लिए मुझे प्रेरित किया। अतः उनके प्रति कृतज्ञता के भाव तथा आभार प्रकट करने के लिए यह कृति विनम्र भाव से उनके ही चरणारविन्दों में उपहार-स्वरूप अर्पित है। गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने, जो योग के एक महान् आचार्य के रूप में संसार-भर में विख्यात हैं, जब ऋषिकेश आश्रम में 'योग-वेदान्त अरण्य अकादमी' की स्थापना की एवं उसके दैनिक वर्ग आरम्भ हुए, उस समय मुझे इन पाठों की शिक्षा देने का आदेश दिया। उपर्लिखित पाठ उस समय बड़ी सावधानी से आशुलिपि में लिखे गये थे जो अब संशोधन, पुनरीक्षण, क्रमबद्ध तथा नव-सम्पादन के उपरान्त इस पुस्तक में उपलब्ध कराये गये हैं।
'योग' शब्द प्रायः ध्यान-मार्ग का अभिधायक है जिसका विवरण राजयोग में दिया गया है। यह (योग) प्रभावकारी एवं सफल ध्यान के सम्यक् अभ्यासार्थ मन को उपयुक्त तथा कार्यक्षम उपकरण बनाने के लिए मन का अनुशासन, प्रशिक्षण तथा पूर्णता-प्राप्ति का प्राचीन विज्ञान है। यह मार्ग अथवा पद्धति पाश्चात्य साधकों को सर्वाधिक रुचिकर है; क्योंकि इसका प्रतिपादन वैज्ञानिक ढंग से किया गया है और इसकी संरचना भी बहुत ही व्यवस्थित है। अन्यच्च, यह सभी मतमतान्तरों का अतिक्रमण करके आपके सम्मुख अपने को किसी भी धार्मिक पद्धति से सर्वथा भिन्न एवं पक्षपात-रहित असाम्प्रदायिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके स्वरूप में ऐसी विधि तथा कला समाहित है जो विश्व के प्रत्येक भाग के लोगों को उपलब्ध है और उनके विश्वास अथवा धर्मानुष्ठान में किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं लाती।
एक सार्वभौम तत्त्व है जिसे जेहोवा, अल्लाह, अहुर्मज्दा, सर्वशक्तिमान् स्वर्ग पिता, ब्रह्म, ताओ अथवा भगवान् आदि विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है। यही विश्वात्मा है जिसकी बन्दना और पूजा मन्दिरों, समाजों, गिरजाघरों, मसजिदों, पारसी-मन्दिरों एवं अन्य सभी पूजा-गृहों में की जाती है। इस सार्वभौम आत्मा की महिमा एवं स्तुति वेद, तालमड, तौर, बाइबिल, कुरान, जेन्द आवेस्ता आदि शास्त्रों में गायी गयी है। राजयोग में इसी विश्वात्मा को ध्याता का ध्येय-विषय कहा गया है। इस पूर्ण वैश्व सत्ता का ध्यान साधक को मन और बुद्धि की चेतना से ऊपर उठा कर परम चैतन्य की अवस्था में ले जाता है, जहाँ वह विषयों के बन्धन से मुक्त हो व्यावहारिक भौतिक सत्ता के प्राण-घातक क्लेशों से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है। यही राजयोग का लक्ष्य है। यह आचार तथा व्यवहार की पवित्रता, अपनी शारीरिक तथा मानसिक प्रकृति की शुद्धि, आत्म-संयम, भक्ति, प्राणमय कोश का सामंजस्य, अन्तर्मुखता, धारणा एवं ध्यान का मार्ग है। इस भाँति इस पथ में ब्रह्माण्डीय तत्त्वों तथा साधक को ईश्वरानुभूति की स्थिति तक उन्नयन करने वाले अध्यात्म के सारभूत अनुशासनों का निगमन है। मेरी कामना है कि सभी पाठक गण इस चरमानुभूति को प्राप्त करें! मैं उनके जीवन एवं साधना में पूर्ण सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। निरन्तर हार्दिक प्रयत्न करते रहने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। अतएव, सााधको ! योग-पथ पर अनवरत अध्यवसाय करो। आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्यमेव होगी।
आशा है कि यह पुस्तक सच्चे जिज्ञासुओं के लिए सहायक एवं लाभप्रद होगी।
यह कृति प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज को समर्पित है और आपको समर्पित है। पूज्य गुरुदेव को मेरा श्रद्धास्निग्ध प्रणाम।
-स्वामी चिदानन्द
विषय-सूची
आध्यात्मिक उन्नति और भगवत्-साक्षात्कार
मन एवं उसके नियन्त्रण-सम्बन्धी कुछ और तथ्य
ध्यान के लिए पूर्वाकांक्षित योग्यताएँ
विषय-प्रवेश
दो मार्ग : प्रेय एवं श्रेय
परम सत्य, परमात्मा को पाने के अभिकांक्षियों ने अपना जीवन एकान्तवास, ध्यान, तपश्चर्या और आध्यात्मिक साधना में व्यतीत किया तथा अन्त में भगवत्-साक्षात्कार-रूपी दिव्य ज्योति को प्राप्त किया। इस प्रकार प्रभासित हो कर उन्होंने भागवत ज्ञान को उद्भासित कर वह मार्ग दर्शाया जो शोक-सन्ताप का अतिक्रमण करके अमरत्व, नित्य-सुख एवं अपरिमित ज्ञान प्रदान करता है—यही मानव-जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है जिसे प्राप्त करके सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है तथा जो मानव-जीवन की भव्यता एवं गरिमा है। मानव-सत्ता के ऐसे सुफल को प्राप्त करके कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। मानव-जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें मुमुक्षुत्व-अनन्त ज्ञान को पाने की प्यास जागृत करनी है और उस ज्ञान के अन्वेषण करने के लिए कर्म करना है जिससे कि हम महान् लक्ष्य का अपनी सत्ता की गहराई में सुस्पष्ट अनुभव कर सकें।
योग-मार्ग में हमें भिन्न-भिन्न साधनाओं का मूल ज्ञान प्राप्त करना है, यथा-वेदान्तियों का ज्ञान-मार्ग, पौराणिक मतावलम्बियों के अनुसार पतंजलि का अष्टांगयोग, शाण्डिल्य एवं नारद द्वारा निरूपित भक्ति अथवा प्रेम-मार्ग और अन्त में परम सत्य की प्राप्ति हेतु पूजा, भक्ति अथवा कर्मयोग का मार्ग गीता-धर्म, जो भगवान् श्रीकृष्ण की भगवद्गीता में आचक्षित है। साधकों को प्रेय-मार्ग[1] से विमुख होना है, जो मनुष्य की केवल भोग-विलास-प्रकृति को ही सन्तुष्ट करता है। यह उसका (मनुष्य का) वास्तविक स्वरूप नहीं। यह (मार्ग) अन्त में अनन्त सुख की ओर नहीं ले जाता और मनुष्य को श्रेय-मार्ग[2] की शरण लेनी पड़ती है जो दिव्य लोक का कठिन मार्ग है, जो विषयों से परे है, जिसमें मन और इन्द्रियों पर संयम की आवश्यकता है, विवेक एवं वैराग्य की आवश्यकता है और जो हमें अमरत्व में ले जाता है।
श्रेय-मार्ग आरम्भ में अप्रिय लगता है; परन्तु अन्त में नित्य-सुख की ओर ले जाता है। प्रेरणादायक कठोपनिषद् में श्रेय एवं प्रेय-मार्ग का भेद बहुत सुन्दर ढंग से बताया गया है। इसमें नचिकेता प्रेय-मार्ग को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करके श्रेय-मार्ग को अपनाते हैं जो कठिन है; परन्तु अन्त में मोक्ष (परमानन्द) की ओर ले जाता है। अतः हमें श्रेय-मार्ग पर ही चलने का इच्छुक बनना है और किसी ऐसे महापुरुष महात्मा के चरण-कमलों की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त करना है जो आभ्यन्तरिक आध्यात्मिक उपलब्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच कर ईश्वर में, परम सत्य में ही संस्थित हो चुका हो।
मानव-जीवन का ध्येय
इस मर्त्यलोक में तीन चीजें प्राप्त करना बहुत कठिन है-मनुष्य- जीवन, मोक्ष की इच्छा एवं प्रबुद्ध जनों की संगति। ये तीनों (वस्तुएँ) केवल प्रभु के आशीर्वाद और कृपा से ही प्राप्त होती हैं। इन तीनों में मनुष्य-जन्म को सर्वप्रथम रखा गया है जो प्रभु की एक अमूल्य देन है। केवल सत्ता के इस स्तर पर ही जीवात्मा प्रज्ञा एवं नित्य-अनित्य-वस्तु-विवेक की दुर्लभ क्षमता से युक्त होता है। अतएव, मनुष्य-जन्म को परमात्मा की एक अत्यन्त दुर्लभ देन माना गया है। मनुष्य-जन्म धारण करके भी यदि आपके अन्दर नित्य-आनन्द एवं अमरत्व को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा जागृत नहीं होती तो इसका अर्थ यह है कि आपने इस जन्म को व्यर्थ ही खो दिया, फिर तो आपका जीना भी पशु-जीवन के समान हो जायेगा। आहार, निद्रा और भोग-विलास का आनन्द लेना, यह सब तो मनुष्य और पशु दोनों में समान है; परन्तु जो चीज मनुष्य को पशु से अलग करती है, वह है मनुष्य का आदर्श, भौतिक सत्ता से ऊपर उठ कर कुछ प्राप्त करने की उत्कट इच्छा। हम जानते हैं कि इस लोक में कोई महत्तर वस्तु प्राप्त करनी है और हमारे अन्दर इस भौतिक जीवन से, अपूर्णताओं के बन्धन से मुक्त होने की तीव्र इच्छा भी है।
इसके पश्चात् है प्रबुद्ध जनों की संगति। पूर्वोक्त दो-मनुष्य-जन्म और मोक्ष की इच्छा होने पर भी हमारा जीवन असफल प्रयासों से पूर्ण एवं मोह-माया से आच्छादित रहता है; क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन-सा प्रयास ठीक है। वह केवल उसी धन्य पुरुष को मिलता है जिसके पास तीसरी देन है प्रबुद्ध जनों की संगति-जो मार्ग के विघ्नों को दूर करती है। यदि हम तत्त्व-ज्ञाता आचार्य के प्रति आत्मार्पण कर दें तो वह हमारा पथ-प्रदर्शन करेंगे। जब रास्ते में मोह-माया हमें व्याकुल करती है तब वह (आचार्य) ही हमें प्रेरणा, उत्साह और साहस दे सकते हैं। इन तीनों से युक्त सौभाग्यशाली व्यक्ति को एक चतुर्थ वस्तु की भी आवश्यकता है, वह है मन, जो कहता है 'ठीक है।' अनियन्त्रित मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। यह माया, मार (काम) अथवा अभिमान का प्रतिनिधि है जो भगवत्-साक्षात्कार के मार्ग में रुकावट बन कर आता है। अतः मन सुप्रसन्न होना चाहिए। आप पर देव-कृपा हो सकती है, गुरु-कृपा हो सकती है, शास्त्र-कृपा भी सकती है; परन्तु जब तक आपको मन का सहयोग प्राप्त नहीं, आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं है।
आध्यात्मिक उन्नति और भगवत्-साक्षात्कार
सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें दिन-प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। अतः वही परम शुभ दिन और पवित्र अवसर है जब हम अपने सब कर्मों को आध्यात्मिक बना कर सर्वरूपेण, ध्यान की उपपत्ति और अभ्यास के लिए नियमित साधना प्रारम्भ कर देते हैं।
हम प्रातः-सायं ध्यान में बैठते हैं; परन्तु दिन-भर अपने कर्मों तथा दूसरों के साथ व्यवहार में मन की क्षुद्रता एवं स्वार्थ प्रकट करते हैं, जो कि हमारी साधना में विघ्न-रूप हैं और ध्यान का लाभ विफल कर देते हैं। यूलिसेस की धर्मपत्नी पेनीलोप के पास उसके पति की अनुपस्थिति में अनेकों लोग उसके साथ विवाह की आशा ले कर आये; परन्तु उसने किसी की भी पत्नी बनना नहीं चाहा। वह एक साध्वी (सुचरित्रा) एवं पतिव्रता स्त्री थी। अतएव उसने आने वाले पुरुषों से कहा कि वह एक वस्त्र तैयार कर रही है और जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता, वह किसी को स्वीकार नहीं करेगी। सब मान गये। वह दिन-भर उस वस्त्र को बुनती और रात्रि में उसे उधेड़ देती। यूलिसेस के आने तक वह ऐसा ही करती रही।
परन्तु हमारे जीवन में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। प्रातः - सायं हम जो भी अभ्यास करें, उसमें कोई अदिव्य तत्त्व नहीं जोड़ना चाहिए। यदि कर्म करते समय हम अपने मूल-तत्त्व को भुला देते हैं, कठोर हो जाते हैं, आलोचना करने लगते हैं अथवा कपटी बन जाते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि ध्यान के समय की हुई साधना को हम स्वयं ही विफल कर देते हैं। अतः हमें बाह्य दैनिक जीवन व गतिविधि के, वाणी और कर्म के समानान्तर हो कर ध्यान, पूजा और साधना के स्तर को उन्नत करना है। ऐसा करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम न केवल शान्त चित्त से कुछ घण्टे साधना में बैठें, अपितु अपने दैनिक कर्मों को भी सद्गुण-सम्पन्न तथा आध्यात्मिक बनायें। हमारे सब कर्मों में हमारे वास्तविक आन्तरिक स्वरूप की झलक मिलनी चाहिए। वे सब कर्म आध्यात्मिक बन जाने चाहिए। कर्मयोग में कर्म की इसी आध्यात्मिकता का शिक्षण दिया गया है। आपको यह ज्ञान होना चाहिए, चाहे आप ध्यानयोगी हों, भक्तियोगी हों अथवा वेदान्ती हों।
कर्मयोग सरल नहीं है। अकेले होने पर तो आपके अन्तर्मन में आदर्श-भाव जागृत हो सकते हैं; परन्तु जब आपको इस विषम संसार में कटु सत्य का सामना करना पड़ता है, उस समय मन की शान्ति बनाये रखना, केवल दैवी गुण दर्शाना और नि:स्वार्थ बनना कठिन हो जाता है। परन्तु यह करने योग्य है, क्योंकि यह योग की अन्य क्रियाओं को सार्थक बनायेगा। आत्म-बलिदान की भावना तथा सर्वतः माधुर्य से पूर्ण आदर्श जीवन-यापन करने वाला व्यक्ति यदि दिन-भर में एक माला भी जप करे तो वह अन्य पुरुषों द्वारा की हुई दस हजार मालाओं के समान है, क्योंकि उसका स्वभाव सात्त्विक कर्मों से पवित्र हो चुका है; किन्तु यदि आपका स्वभाव काम-क्रोध से युक्त है, तो आप चाहे ध्यान में भी क्यों न बैठें, क्षेत्र तैयार न होने के कारण आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको आश्चर्य होता है- 'मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है?' ऐसा इसलिए कि नित्य कर्मशील जीवन में आप साधना से विरोध कर रहे हैं। साधक को बुद्धिमान् होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि बरतन में छिद्र कहाँ है; अन्यथा छेद वाले बरतन को वह भरने का यत्न करता रहेगा और उसका यत्न निरर्थक होगा। उसको उस छिद्र को ढूँढ़ना है तथा इसके लिए कर्मयोग की कला उसको सीखनी है। इन सब बातों का उसको अभ्यासकृत ज्ञान होना चाहिए।
प्रणव अथवा ॐ शब्द का उच्चारण अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। यह हमें स्मरण कराता है कि हम वास्तव में 'कौन' हैं। हम इस शरीर, मन और प्राण को ही अपना स्वरूप समझते हैं। 'प्रणव' हमें याद दिलाता है कि हम वास्तव में क्या हैं? ॐ शाश्वत है, अगाध शान्ति है, परम ज्योति-स्वरूप है, ज्ञान है, सच्चिदानन्द है, नित्य-शुद्ध है, नित्य-बुद्ध है। यह ही वास्तव में हम हैं। प्रभु की अनिर्वचनीय माया के कारण हम निज स्वरूप को भूल गये हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं- 'हमें पीड़ा है', जब कि पीड़ा शरीर में होती है। हम कहते हैं- 'हममें अशान्ति है', जब कि विषण्णता हमारे मन में है। यह भूल शरीर और मन के अध्यास के कारण है। अतएव हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराने और आत्म-चैतन्य में संस्थित होने के लिए विविध योग-मार्ग हैं। सब योग-मार्गों तथा आध्यात्मिक संघर्षों का अन्तिम लक्ष्य केवल मात्र आनन्दमय आत्म-तत्त्व की अनुभूति है। अतः प्रणव अर्थात् ॐ हमें याद दिलाता है कि प्राप्त करने योग्य चरमानुभूति कौन-सी है? ॐ का साक्षात्कार ही योग का चरम फल है और इसे निरन्तर याद रखने के लिए हम ॐ का उच्चारण करते हैं जो हमें मनः प्रसाद प्रदान करता है। यद्यपि, युगों तक आप माया-जनित भ्रम में क्यों न पड़े रहे हों, तथापि सत्य के संस्पर्श से आप मनःप्रसाद अनुभव करेंगे। महान् सत्य की उपलब्धि का यही गौरव है।
योग का रहस्य केवल भोग का त्याग नहीं है, अपितु महाभोग (सब भोगों के भोग) की प्राप्ति है। योगी जानता है कि यदि त्रिलोक के समस्त सुख एकत्र करके एक पलड़े पर रख दिये जायें और दूसरे पलड़े पर आत्मा के परम आनन्द-स्वरूप का अति-सूक्ष्म कण भी रखा जाये तो दूसरा पहले से कहीं भारी होगा।
वह मानव सचमुच में ही विज्ञ है जो योग के हेतु इन्द्रिय-सुख का त्याग करता है। यह स्वर्ण-प्राप्ति के लिए जाली सिक्का फेंकने के समान है। वह जानता है कि वह फेंक तो कुछ भी नहीं रहा; परन्तु इन्द्रिय-सुख त्याग कर जो उसे प्राप्ति होती है, वह अद्वितीय है। अतः योग मुख्यतः परम आनन्द की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला एक प्रयास है। यह एक विशेष दृष्टिकोण से योग की एक परिभाषा है। इसकी और परिभाषाएँ भी हैं। कुछ नकारात्मक एवं सकारात्मक परिभाषाएँ भी हैं।
एक शिशु माँ को सीते हुए देखता है। वह देखता है कि माँ अंगुलि पर अंगुलित्राण चढ़ा रही है। वह पूछता है- 'माँ, तुम अंगुलित्राण क्यों चढ़ा रही हो?' फिर माँ समझाती है कि यह इसलिए पहना जाता है कि कभी अकस्मात् ही अंगुलि में सुई चुभ जाये तो उससे पीड़ा अथवा रक्त-प्रवाह न हो। योग में भी हम ऐसे ही अभ्यास की चेष्टा करते हैं। आपको योग के सम्बन्ध में कुछ अधिक विस्तार में बता रहे हैं। इतिहास से बहुत पूर्व सृष्टि के आरम्भ में मानव को एक पुरातन आवश्यकता की अनुभूति हुई। वह क्या थी ? महात्मा बुद्ध के जीवन में यह बात बहुत निश्चित रूप से प्रतिपादित हुई है। उनका सम्पूर्ण दर्शन 'निर्वाण' पर आधारित है। सांसारिक प्राणियों को दुःखी देख कर उन्होंने एक प्रयोजन की पूर्ति के हेतु प्रयास किया। इतना ही नहीं, पुरातन काल में भी पूर्वजों ने मनुष्य-जीवन का परीक्षण किया और इसे दोषपूर्ण एवं दुःखमय पाया। इससे उनके मन में संघर्ष उत्पन्न हुआ। उन्होंने जिज्ञासा की कि 'क्या इन अपूर्णताओं और सीमाओं को पार करने का कोई उपाय है? क्या इन दुःखों और क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करने का कोई साधन है?' उन्हें ज्ञात हुआ कि यह शरीर अन्ततः षड्-विकारों का शिकार है-उत्पत्ति, शरीर-वृद्धि, बालपन, प्रौढ़ता, वृद्धता और मृत्यु। जन्म-मृत्यु के छोरों के बीच का समय जीवन है। अतः इस अनिश्चित काल में व्यक्ति जो भी थोड़ा-बहुत इन्द्रिय-सुख प्राप्त कर सकता है, उसमें व्याधि, परिवर्तन और क्षय विघ्न-रूप में सामने आते हैं। क्या इस अपूर्ण भौतिक जीवन में परित्राण पाने का कोई उपाय है?
हमारे पूर्वज बहुत व्यावहारिक थे। आज भी सच्चा हिन्दू बड़ा व्यावहारिक है। भले ही लोग उसे अव्यावहारिक तथा अयथार्थवादी समझते हैं; पर यह एक रोचक विषय है कि वह बहुत ही व्यावहारिक है। यदि वह यह समझता है कि अमुक वस्तु परिश्रम और प्रयत्न के योग्य है तो उसके लिए अपने जीवन तक की आहुति देने को उद्यत हो जाता है। बाह्य जीवन को मूल्यहीन समझ कर हिन्दू इसका त्याग करने को तैयार हो गया। लोगों को लगा कि वह स्वप्न देख रहा है। क्या संसार की अपूर्णताओं से मुक्ति प्राप्त करने का भी कोई साधन है? व्यावहारिक हिन्दू-मन ने तुरन्त अन्वेषण आरम्भ किया। निरन्तर परिश्रम के द्वारा उसने मानव-सत्ता की गहराई में प्रवेश किया और महान् अतीन्द्रिय सत्य का साक्षात्कार किया। सब क्लेशों एवं सीमितताओं से परे, सर्व बन्धनों से मुक्त उसको पा कर परमानन्द के दिव्य भावावेश में निमग्न हो गया। सर्वोच्च अनुभव के अनन्तर उसने मर्त्यलोक को सम्बोधित करके कहा- "हे मानव ! नित्य कल्याण की ओर ले जाने वाले मार्ग का मैं तुम्हें दर्शन कराऊँगा। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊँगा जो दुःख से परे ले जायेगा।"
मानुषिक जीवन एवं इसे आकुलित करने वाले सन्ताप, दुःख और क्लेशों का पर्यवेक्षण तथा सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात् हमारे पूर्वजों के मन में आग्रह उत्पन्न हुआ ऐसा मार्ग ढूँढ़ा जाये जो इन सब (दुःख आदि) का अतिक्रमण कर सके। दोष-रहित जीवन (बनाने) के लिए उपाय खोजना उन्होंने अत्यावश्यक समझा। इस अभाव की पूर्ति हेतु योग-विद्या आयी, जो आपको दुःखों से मुक्त करके आप पर अविरल आनन्द की वर्षा करती है। योग-क्रियाएँ सर्व दुःख-निवृत्ति एवं परमानन्द-प्राप्ति के लिए अति-प्रभावशाली हैं। ये आनन्द ही नहीं, परमानन्द की प्राप्ति कराती हैं। मनुष्य की एक गहरी चाह के परिणाम-स्वरूप योग-विद्या का आविष्कार हुआ, जब मनुष्य ने अपने अस्तित्व की पीड़ा का अनुभव किया और ऐसा मार्ग ढूँढ़ना चाहा जो उसे दुःख से परे ले जाये; सब अपूर्णताओं, सीमाओं, मलिनताओं, स्थूल एवं भौतिक सत्ता से परे ले जा कर उस उच्चतर चिन्मय तत्त्व का दर्शन कराये जिसमें उसे असीमता, शान्ति एवं पूर्णता के नित्य-जीवन का अनुभव हो।
इस दृष्टि से अन्य प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आखिर हमें योग का अध्ययन किस हेतु करना चाहिए? भौतिक संसार की इन अपूर्णताओं और क्लिष्ट बन्धनों से कौन पूर्णतया मुक्ति नहीं चाहता? परमानन्द और दिव्योल्लास का सुखास्वाद कौन नहीं लेना चाहेगा? वह व्यक्ति मूर्ख है जो यह सब नहीं चाहता। वह महामूर्ख है जो अपना जीवन व्यर्थ में गँवाता है। ऐसा व्यक्ति तो दया का पात्र है। वह उल्लू की तरह आँखें बन्द कर लेता है और कहता है- "मुझे प्रकाश नहीं चाहिए।" परन्तु जब कि दुःखों का अतिक्रमण करने का साधन विद्यमान है, इस तरह कहना बुद्धिमत्ता नहीं है-"ओह! आश्चर्य! इस भौतिक संसार में लोग अमृत को अस्वीकार कर विषपान करते हैं।" यदि कोई योग को अस्वीकार करके भोग का आनन्द लेता है तो बुद्धिमान् व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा। योग का यही महत्त्व है। यह मनुष्य को दुःखों से छुटकारा दिला कर उस पर अविरत आनन्द, आत्म-चेतना (जिसका स्वरूप आनन्द है) की वर्षा करता है।
योग का थोड़ा-सा ज्ञान भी हमें महान् आन्तरिक शक्ति प्रदान करता है; क्योंकि इससे मनुष्य को अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। अतः जीवन के लिए यह एक गौरवपूर्ण मार्ग है-ऐसा मार्ग जो मार्ग मानव-सत्ता के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति करता है। अतएव योग के प्रति सबको अभिरुचि होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग क्लेशों से मुक्त हो कर शान्ति एवं आनन्द में निवास करना चाहते हैं।
योग की मौलिक संकल्पना
जैसा कि पहले ही निर्दिष्ट हो चुका है, योग मनुष्य की किसी अभाव-पूर्ति के परिणाम-स्वरूप सामने आया। पूर्वजों ने अनुभव किया कि यह जीवन सीमित तथा अपूर्ण है। मानव-मन में सर्वदा कुछ अभाव अथवा अपूर्णता की भावना रहती है जिसे वह पूरी करना चाहता है। बाह्य भौतिक पदार्थों से इन्द्रियों द्वारा यथा आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा से मनुष्य को सन्तुष्टि मिलती है। उसमें सदा दुःख और दर्द छिपा रहता है। प्रथमतया, तृष्णा पीछा नहीं छोड़ती और जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, मनुष्य को मानसिक शान्ति नहीं मिलती। अतः उस इच्छा की पूर्ति के लिए उद्यम आरम्भ हो जाता है। यदि प्रयास असफल रहता है तो वह निराश हो जाता है। इच्छा-पूर्ति के हेतु प्रयास के समय यदि और कोई विरोध कर दे तो वह क्रोधित हो उठता है। यदि किसी दूसरे मनुष्य के पास वह पदार्थ है जो उसके पास नहीं है तो उसमें ईर्ष्या उत्पन्न होती है। बहुत प्रयत्न करके और सब विघ्नों का अतिक्रमण करने के पश्चात् उसे कोई वस्तु यदि प्राप्त भी हो जाती है, तो उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं वह उसके हाथ से निकल न जाये। फिर चिन्ता जाग्रत होती है उस पदार्थ को सुरक्षित रखने की। चिन्ता और भय, जहाँ ये दो मिल जायें, वहाँ शान्ति हो ही नहीं सकती।
इतने परिश्रम, भय तथा चिन्ता के पश्चात् यदि प्राप्त पदार्थ हाथ से निकल जाये तो दुःख होता है। किसी पदार्थ के प्रति मन के मोहित होते ही इच्छा उत्पन्न होती है। प्रयत्न, चिन्ता, भय, निराशा, दुःख -सब उसका अनुसरण करते हैं। मन अशान्त रहता है। मन की स्वाभाविक प्रकृति ही इच्छा है। निरन्तर विचार-प्रवाह आरम्भ होता है और सद्यः विचार कल्पना में बदल जाते हैं तथा यही कल्पना इच्छा का रूप धारण कर लेती है। इसके अनन्तर इच्छा-शक्ति रंग में आती है और वह हाथ-पैर आदि विभिन्न अंगों को इच्छा-पूर्ति के लिए आज्ञा देती है। स्मृति से विचार उत्पन्न होते हैं और विचार कल्पना की सहायता से एकदम इच्छा में परिवर्तित हो जाते हैं। इच्छा होने पर मन क्रियाशील हो जाता है। 'मैं इसे कैसे पूर्ण करूँ ?' ऐसा भाव उदित होता है। अब अहंभाव उत्पन्न होता है, फिर दृढ़ निश्चय की क्षमता भी प्रकट होती है। उसके पश्चात् कर्म, उद्यम, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिन्ता और निराशा अनुसरण करते हैं। निराशा तब मिलती है जब हमारा संकल्पित पदार्थ हमारी आशा की अपेक्षा के रूप में नहीं मिलता; परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। हम गलत सोचते हैं। निनानवे प्रतिशत लोगों के साथ ऐसा हुआ है।
विचार एक वस्तु है; परन्तु उसका वास्तविक अनुभव दूसरी वस्तु है। अन्ततः हमें ज्ञात होता है कि सब नाम एवं रूप नश्वर हैं और सब सम्बन्ध अल्पकालिक हैं। मृत्यु के समय जब सब पदार्थ हमें छोड़ देते हैं तो दुःख का अनुभव होता है। इन्द्रियों को वश में करके, इन्द्रिय-विषय-सुख की इच्छा से मुक्त हो कर हमें दुःखों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन्द्रियों पर संयम किस प्रकार किया जाये और मन के निष्ठुर शासन से स्वयं को कैसे मुक्त किया जाये-यह सब योग में सिखाया गया है। दुःख, चिन्ता और निराशा से दूर शाश्वत आनन्द का अनुभव हमें योग द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।
हमें देखना है कि योग के मूल-तत्त्व क्या हैं? मन विषयों की ओर ही क्यों भागता है और इच्छा उसकी प्रकृति क्यों है तथा क्या मन की क्रिया को रोकना सम्भव है? इनका विचार हमें आगे करना है। प्राचीन युग में लोगों ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि इस दुःखदायी और सीमित अनुभव देने वाले मन का क्या किया जाये। उन्होंने प्रयास कैसे आरम्भ किया? वह कौन-सा तत्त्व है जिसे योग द्वारा क्रियाशील बनाया जा रहा है? यहाँ हमें मानुषिक दशा का विचार करना है। उन्होंने प्रतीति की कि मनुष्य तीन पदार्थों का एक विचित्र मिश्रण है। हम सब जानते हैं, हम सोचते हैं, हम क्या हैं और अपनी मेधा (बुद्धि), युक्तिपरायणता और तर्कशीलता का प्रयोग करते हैं।
मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अतः हम स्वयं को मनुष्य के रूप में पहचानते हैं जो विचार कर सकता है, अनुभव कर सकता है, अनुमान लगा सकता है, नवीन निर्णय ले सकता है तथा ज्ञान से युक्त है। तथापि, समय आता है जब कुछ विशेष परिस्थितियों में हम अपनी बुद्धि और तर्क को भूल कर बहुत कुछ पशु के समान बन जाते हैं। जब क्रोध अथवा ईर्ष्या का प्रचण्ड आक्रमण होता है, हम किसी भी पशु की भाँति बन जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि मनुष्य की रचना में ही कुछ भाग अपमानव, अशुद्ध अथवा पूर्णरूपेण पाशविक है, यद्यपि शताब्दियों-पर्यन्त परिमार्जन के पश्चात् मनुष्य का उद्विकास हुआ है और मानव-जाति के इस सामूहिक विकास के परिणाम-स्वरूप ही अपमानवता दब गयी है। बहुत क्रोध आने पर मनुष्य किसी की हत्या भी कर सकता है जो कि सामान्य मनःस्थिति में वह नहीं करेगा। कुछ समय पश्चात् वह स्वयं ही हैरान रह जाता है और सोचता है, 'क्या मैं यह कार्य भी कर सकता था ?' व्यक्ति में मानवीयता एवं संयम के समाप्त होने पर पाशविक (अपमानवता की) प्रवृत्ति पूर्णतया आच्छादित हो जाती है; यह सबका अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने यह ज्ञात किया कि यह भी मनुष्य का मौलिक अंश है; परन्तु कुछ मनुष्यों में यह दबा हुआ है। जहाँ जाति का विकास नहीं हुआ वहाँ यह अंश आज भी क्रियाशील है। मनुष्य-रूप में होने पर भी ये सर्वथा पशु-समान हैं। दार्शनिक भाषा में मनुष्य का यह भाग 'अधम आत्मा' कहलाता है। तान्त्रिक भाषा में इसे 'पशु' कहा जाता है, जब कि वेदान्त इसे 'अशुद्ध मनस्' कहता है जो मल तथा पाशवी लक्षण द्वारा चित्रित किया गया है और पशु का लक्षण है।
यह अशुद्ध मन तो प्रत्येक में है, कभी संयमित अवस्था में और कभी असंयमित अवस्था में। हमें तो केवल इतना ही स्मरण रखना है कि वास्तविक मनुष्य यह शरीर, मन अथवा बुद्धि नहीं है। सत्य तो यह है कि मनुष्य आत्म-तत्त्व है। वह तत्त्वतः अविनाशी है; सत्य, ज्ञान और आनन्द से भरपूर है। यही मानव का मूल-स्वभाव है-शुद्ध सच्चिदानन्द। उसकी मूल-प्रकृति पत्थर के टुकड़े के समान जड़ नहीं है। वह जानता है- 'मैं वही आनन्द-स्वरूप हूँ।' आत्म-जागृति में ही मनुष्य का अस्तित्व है। सत्-चित्-आनन्द आप सबके वास्तविक स्वरूप की परिभाषा है; परन्तु यही चैतन्य मन और इन्द्रियों से आच्छादित हो जाता है और आप कहते हैं- 'मैं यह काम कर रहा हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं सुखी हूँ' इत्यादि। आप स्वयं को शरीर एवं मन से एकरूप समझ लेते हैं।
मनुष्य तीन तत्त्वों से बना है। उसमें सारभूत वास्तविक दिव्यता है। इसके उपरान्त पशु-प्रकृति है जो तमोगुण, अन्धकार आदि से भरी है। इन दोनों के बीच में मानव-प्रकृति है। कभी तो सत्संगति से उसमें पवित्र भावनाओं का आगमन होता है और कभी कुसंगति से उनके मन में बुरे विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं और वह उस स्थान से बाहर आना चाहता है। मनुष्य विशुद्ध एवं अशुद्ध आत्म-तत्त्व के मध्य दोलित रहता है। एक ओर से उसके उच्च आध्यात्मिक तत्त्व का आकर्षण होता है और दूसरी ओर उसकी अधोमुख पाशविक वृत्ति का। उसकी अपनी बुरी आदतें, सहयोगी वातावरण आदि उसे निम्न दशा में बाँधे रखते हैं। अतः योग का मूल उद्देश्य, किसी भी भाँति मनुष्य की पाशविक वृत्ति का, उसके अधम तत्त्व का शोधन करना है। प्रत्येक बार मनुष्य का आध्यात्मिक तत्त्व उसे ऊपर ले जाना चाहता है; परन्तु अधम तत्त्व उसे अपनी ओर खींचता है। योग का प्रयोजन ही शोधन करना है जिससे कि दिव्य चैतन्य के प्राकट्य में कोई विघ्न न रहे। मन शुद्ध होने पर ही दिव्य चैतन्य का साक्षात्कार होता है। मन के पूर्णतया शुद्ध हो जाने पर हम उस आनन्दमय आत्म-तत्त्व का दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा मूल-स्वभाव है। इसे निज-स्वरूप कहा जाता है। इस समस्या के सन्दर्भ में यह तर्क सामने आता है कि 'राजयोग' भी मनुष्य की मलिनता को दूर करके उसे दिव्य बनाने के लिए शिक्षण दे सकता है और सभी योग विभिन्न प्रकार से यही शिक्षा देते हैं।
वेदान्त के अनुसार मल, विक्षेप और आवरण- ये तीन प्रतिबन्धक हैं जो जीव को बन्धन में डालते हैं। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ एवं काम मनुष्य की मलिनताएँ हैं और ये उसके शरीर के साथ एकरूपता में केन्द्रित हैं। अतः प्रथम तो स्थूल भौतिक व्यक्तित्व को दूर करना है। द्वितीय बाधा है विक्षेप-मन का आन्दोलन। मन किसी एक विचार अथवा विषय पर कभी भी एकाग्र नहीं रह सकता। वह सदा एक पदार्थ से दूसरे की ओर भागता रहता है। अभी यह कनाडा में है तो थोड़ी देर में यह जर्मनी अथवा अमरीका में होगा। मन की तो यह चंचल प्रवृत्ति विक्षेप कहलाती है। अतः योग-शास्त्र कहते हैं कि यदि आपको अपनी निम्न प्रकृति में शुद्धि लानी है तो 'विक्षेप' से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। आप इतना कर लेते हैं तो इससे आगे मोह-माया से भी आपको छुटकारा पाना होगा, जिसके कारण आप सोचते हैं कि आपका स्वरूप यह शरीर ही है। यह भ्रम, जिसे 'अविद्या' भी कहते हैं, परम सत्य के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल देता है।
महर्षि पतंजलि ने कहा- 'यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने स्वभाव की शुद्धि करनी होगी और अवांछित गुणों का बहिष्कार करना होगा।' अतः सदाचार एवं सद्गुणों के विकास की शर्त को उन्होंने राजयोग का प्रथम सोपान बनाया। साधक को सदाचार का साकार रूप होना चाहिए। यही नींव है जिस पर साधना-मन्दिर का निर्माण होगा। गुण कितने हैं? यदि आप स्वामी शिवानन्द जी की पुस्तकों का अध्ययन करें तो आपको शतशः गुण मिलेंगे, जो एक अभिकांक्षी में होने चाहिए। पतंजलि ने इस समस्या का समाधान सहजावबोधपरक (Intuitive) विधि से किया है। उन्होंने पाँच मूल गुण चुने जो अच्छाई के विपुल स्रोत हैं। यदि आप दृढ़तापूर्वक स्वयं को इन पाँच गुणों में संस्थित कर लें तो शेष सब गुण आपमें स्वतः आ जायेंगे।
यदि आप सेना के कमाण्डर को पकड़ लें तो समस्त सेना आपकी वशवर्ती हो जायेगी; वैसे ही उन्होंने कहा- "पाँच मौलिक (सारभूत) गुणों का अनुष्ठान कीजिए। उनमें दक्षता प्राप्त कीजिए। तब आपकी सम्पूर्ण प्रकृति ही सद्-स्वरूप हो जायेगी। सद्गुणों में यही शक्ति है।" अष्टांगयोग के प्रथम पाद से जिन पाँच मौलिक गुणों का अनुष्ठान होता है उन्हें 'यम' कहा जाता है। उनमें प्रथम है 'अहिंसा' - किसी को हानि न पहुँचाना। किसी को दुःखी मत करो, पिपीलिका अथवा पौधे को भी नहीं। शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु किसी को दुःखी करने की मन से भी न सोचो। किसी भी जीव को भयभीत करने अथवा दुःख देने का स्वप्न भी मत देखो। मनुष्य को साधु अथवा पूर्णतया गुणी बनाने के लिए यह एक गुण ही पर्याप्त है।
दूसरी विशेषता है 'सत्य'। सत्य में ही निवास करो। जीवन से भले ही हाथ धोना पड़े, पर सत्य के विरुद्ध मत जाओ। झूठ की शरण मत लो। कोई ऐसा कार्य मत करो जो 'सत्यता' के विपरीत हो। आप सोचें कुछ, बोलें कुछ और करें कुछ-मनसा-वाचा-कर्मणा में ऐसा अन्तर न कीजिए।
अब आता है 'ब्रह्मचर्य' -विचार, वाणी एवं कर्म में शुद्धता। महिलाओं की दृष्टि से तो यह सतीत्व है। चतुर्थ है 'अस्तेय' अथवा चोरी न करना। जो वस्तु दूसरों की है, उसे लेने का प्रयत्न मत करो। पड़ोसी के धन का लोभ मत करो। दूसरे के पदार्थ का हरण कभी मत करो। यदि सब देश इसका पालन करने लगें तो कभी लड़ाई तथा युद्ध नहीं होंगे। अन्तिम है 'अपरिग्रह' अर्थात् ऐश्वर्य का त्याग। दूसरे से किसी भी ऐश्वर्यप्रद वस्तु को स्वीकार मत करो।
इस प्रकार राजयोग का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण रूप से सदाचारी बनाना है। राजयोग के प्रथम सोपान पर अभिकांक्षी को पाँच गुणों से सम्पन्न होना है-अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य (शुचिता), अस्तेय एवं अपरिग्रह। विश्व-प्रेम और निःस्वार्थ सेवा मनुष्य को साधु-जीवन में संस्थित कर देगी जो राजयोग के उत्तर सोपानों के निर्माण में नींव-स्वरूप काम करेगा।
अन्तरंग-योग
मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसकी (मानुषिक) प्रकृति विवेक-शक्ति में ही निहित है और यही उसके स्वत्व का केन्द्र भी है। उसका शुद्ध, पूर्ण, दिव्य सत्त्व जो अजेय, अजन्मी, अक्षय, अविनाशी तथा अमर सत्ता है, जो मानव की वास्तविक सत्ता है, जो मन के निष्क्रिय हो जाने पर भी बनी रहती है-मानव को चेतना के ऊर्ध्व सोपानों के प्रति आग्रह करती है। भौतिक शरीर के नष्ट होने पर जब जीवनावधि समाप्त हो जाती है तो मानसिक क्रियाएँ और सब इन्द्रियों के कार्य भी, जो विचार-प्रवाह पर आधारित होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मन के निष्क्रिय होने पर भी मनुष्य का वास्तविक तत्त्व चेतन (आत्मा) अमर रहता है। आत्म-साक्षात्कार करने वाले ऋषियों की खोज़ से प्रतीति हुई है कि इस चैतन्य की यह इकाई एक श्रृंखला की कड़ियों के साथ क्रमशः घूमती ही रहती है। इस श्रृंखला में अवतार भी एक कड़ी होने के कारण शरीर के क्षय एवं मन के निष्क्रिय होने के पश्चात् चैतन्य के सातत्य-सम्बन्धी संशय दो रूपों में व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। व्यक्ति में पूर्व-जन्म की स्मृति सक्रिय रूप में पायी गयी और उसके द्वारा पूर्व-जन्म के बताये हुए तथ्य परीक्षण के उपरान्त अक्षरशः सत्य पाये गये। पश्चिमी देशों के कुछ अन्वेषकों द्वारा जो शरीर के क्षयोपरान्त व्यक्तिगत सम्पर्क सिद्ध हो सका, वह थोड़ा निम्न स्तर का प्रमाणित हुआ।
उच्चकोटि के व्यक्तियों में, जिन्होंने चैतन्य की निरन्तरता का प्रतिपादन किया, श्री ओलीवर लाज आदि का नाम उल्लेखनीय है। पश्चिमी साहित्य एवं विचारकों में वे बहुत प्रसिद्ध थे। मानव का यह तात्त्विक अंश सदा उसे दिव्य आकांक्षाओं एवं उच्चतर चैतन्य की ओर पहुँचने को अग्रसर करता रहता है जिसमें संस्थित होने पर अन्नमय तथा मनोमय कोशों के दुःख और क्लेश उसे व्याप्त नहीं हो सकते। वह अवस्था अविरल आनन्द की अवस्था है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मनुष्य के चेतन स्वभाव के अतिरिक्त उसके अस्तित्व का एक और पक्ष भी है-नृशंस पाशवी पक्ष, जो विषयों में रुचि रखने वाला, भोग-विलास की इच्छा रखने वाला एवं कुरुचि से युक्त है।
सांसारिक प्रक्रिया जीव-सत्ता के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर उत्थान है। भारतीय विचारधारा के अनुसार जैसे ही व्यक्तिगत चेतना की इकाई अस्तित्व के निम्न स्तर की अवस्था से गुजरती है, उसमें उस अवस्था के संस्कार चेतना में गहराई तक अंकित हो जाते हैं और यही उसकी पाशवी प्रकृति अथवा अशुद्ध स्थूल अस्तित्व का सृजन करती है। इस प्रकार अस्तित्व का प्रत्येक स्तर उसके भीतर अपनी प्रकृति का कुछ-न-कुछ चिह्न छोड़ता जाता है। पाशवी अवस्था में मूल-प्रकृति प्रधान है जो उत्तेजना के रूप में निहित रहती है और उस पर जीव का वश नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति विवेक द्वारा संयमित नहीं होते, अतएव वे निम्न स्तर की जीव-सत्ताएँ कही जाती हैं। पशुता चैतन्य द्वारा वशीभूत एवं दमित हो जाती है। दिव्य तत्त्व को, जो अभी सुप्त रूप में है, जाग्रत होना होता है। बीच में है मानव-प्रकृति, सर्वदा क्रियाशील गत्यात्मक शक्ति-सम्पन्न जो व्यक्ति के जीवन में स्वयं को विभिन्न आकारों में व्यक्त करती हुई पशु-प्रकृति और देव-प्रकृति के बीच में शासन करती है। प्रत्येक जीव हठात् ही वशीकृत, परन्तु क्रियाशील पशु-प्रकृति की ओर बलपूर्वक खिंचता है। प्रत्येक मनुष्य में पशु-प्रकृति विभिन्न रूपों में क्रियाशील होती है, जब कि दैवी प्रकृति अभी गतिशील ही नहीं हुई है। वह अभी सुप्त है, जाग्रत नहीं। अतः व्यक्ति निरन्तर पाशवी प्रकृति की ओर खिंचा चला जाता है।
मानव-जीवन व्यक्ति की अदिव्य प्रकृति एवं विवेक-शक्ति के बीच एक संघर्ष मात्र है जो कहती है- 'मेरे विचार में यह (करना), मेरे योग्य नहीं। मानव होने के नाते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।' ये विचार मनुष्य के विवेक द्वारा सदा क्रियाशील रखे जाते हैं। कैसे ? प्राथमिक शिक्षण के प्रभाव द्वारा। बाल्यावस्था में बड़े लोग आपको कुछ कामों के लिए, तो मना करते हैं और कुछ कार्यों के सम्बन्ध में कहते हैं कि ऐसा कार्य लज्जाजनक है। प्राथमिक शिक्षण एवं पारिवारिक संस्कार बहुत महत्त्व रखते हैं। मान लीजिए, आपका जन्म एक सुशिक्षित, शिष्ट परिवार में हुआ है। स्वभावतः आपकी प्रवृत्तियाँ अधिक शुद्ध होंगी। इसी कारण से, अशिक्षित एवं पिछड़े हुए परिवार में जन्म लेने वालों में संयम की कमी होती है। यद्यपि उनमें तर्क-शक्ति तो होती है; परन्तु इतनी नहीं जितनी एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत परिवार में जन्म लेने वाले मनुष्य में होती है। प्रारम्भिक शिक्षण, पैतृक ज्ञान, तदनन्तर आपके पूर्व-संस्कार क्रियाशील होते हैं।
पूर्व-जन्म का प्रभाव ही संस्कार कहलाता है। प्रगति ही जीवन है और प्रत्येक जन्म में मनुष्य कुछ सीखता है और अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करता है। यह सब ज्ञान मनुष्य में संस्कार-रूप में रहता है। संस्कार-यह ऋण हो या सम्पत्ति जो किसी पूर्व-जन्म के अनुभवों या कर्मों से प्राप्त की गयी है, अहंभाव अथवा व्यक्तित्व द्वारा कार्यशील होते हैं और एक विशेष आयु के उपरान्त मनुष्य में कार्य करना आरम्भ कर देते हैं।
बचपन में व्यक्तित्व कार्य नहीं करता। साधारणतया एक विशेष आयु के पश्चात् ही बच्चों का व्यक्तित्व प्रस्फुटित होता है और ऐसा करने पर उनके पूर्व-जन्म के संस्कार कार्य करना आरम्भ करते हैं। वे मनुष्य के तर्क-वितर्क में भी भाग लेना आरम्भ कर देते हैं और मनुष्य को कुछ काम करने के लिए उत्तेजित करते हैं तथा कुछ से बचने के लिए कहते हैं। हमें सभ्य समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। लोग कहते हैं- 'यह मत करो।' कुछ कार्यों का निषेध है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें घृणित समझा जाता है। ये ही प्रभाव मानव के विवेकशील पक्ष का निर्माण करते हैं। यह तत्त्व तथा निम्न स्तर की कामनाओं का परस्पर संघर्ष ही प्रत्येक व्यक्ति में द्वन्द्व उत्पन्न करता है। मनुष्य में आत्म-सम्मान तथा शिष्टाचार की भावनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं और कुछ सीमा तक, वे उसकी स्थूल पाशवी प्रकृति को संयम में रखती हैं। यदि वह किसी विशिष्ट चिन्तक के सम्पर्क में आता है, ज्ञान के वचन सुनने लगता है, उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन करने लगता है और अधिक-से-अधिक आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनने लगता है तो उसकी प्रज्ञा (बुद्धि) शिक्षित होने लगती है, अधम वृत्तियों पर संयम दृढ़ होने लगता है और उसको मानुषिक बनाने लगता है और वह एक ऐसा इन्सान बन जाता है जिसमें आत्म-संयम है, आत्म-अनुशासन है, अपनी अधम वृत्तियों और कामेच्छाओं पर संयम है।
कभी तो समाज का भय भी मन को अधर्म तथा निम्न कोटि की वासनाओं को तृप्त करने से रोकता है। मान लो कोई व्यक्ति अनुचित कार्य करता है तो समाज उसे दण्ड देता है। अतः दण्ड का भय लगा ही रहता है। विकास के उच्च स्तर पर मनुष्य को संसार का नहीं, अपितु सार्वभौमिक नियमों के विरुद्ध चलने पर दण्ड का भय रहता है। ये सब बातें मनुष्य को पूर्णरूपेण मनुष्यता के स्तर पर ले आती हैं तथा पाशवी वृत्तियों के अनवरत प्रदर्शन पर रोक लगाती हैं।
और फिर अक्सर विरोध भी उत्पन्न होता है। कभी अकस्मात् ही मनुष्य के जीवन में कोई ऐसा क्षण आ जाता है जब वह गम्भीरतर रूप से विचार करना आरम्भ करता है साधु बनने के लिए, ऊँचा उठने के लिए और 'उसका' अनुभव करने के लिए जो लौकिक, स्थूल अथवा शारीरिक नहीं है। ऐसे समय में मनुष्य दार्शनिक बन जाता है और विषय-वासनाओं के जीवन से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है; किन्तु पुनः अपने दैनिक कार्यक्रम के भँवर में फँसने पर वह जीने का यथार्थ उद्देश्य भूल जाता है। एक बार फिर उसके जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब वह पूछता है- 'क्या जीवन में कोई उच्चतर लक्ष्य भी हैं?' यह भाव मनुष्य के अनुभव तथा आत्म-साक्षात्कार करने योग्य उच्च तत्त्व की क्षमता की ओर इंगित करता है।
उठी हुई इस तरंग से मनुष्य लाभ उठाता है और भौतिक संसार की दैनिक उथल-पुथल से ऊपर उड़ने योग्य हो जाता है। इसी के लिए सन्त और सिद्ध पुरुष उसे निरन्तर यह कहते हुए उत्साहित करते हैं : 'तुम यहाँ क्या कर रहे हो! कब तक निद्रा में पड़े रहोगे?' वे सुप्त परन्तु महत् दैविक प्रकृति को पुनः-पुनः जागृत करने का यत्न करते हैं। मानव की त्रिगुण प्रकृति का विश्लेषण करने पर हमें ज्ञात होता है कि योग-मार्ग में जो प्राप्त करने योग्य है, वह है-अधम, पाशवी प्रकृति का दमन अथवा विनाश तथा आत्म-तत्त्व का परमात्म-तत्त्व में उदात्तीकरण, जहाँ वह शरीर और मन की सीमाओं से दूर पहुँच कर अपनी आनन्दमय शाश्वत प्रकृति-अन्तःकरण में आलोकित होने वाले नित्य सत्य में संस्थित हो कर अविरल आनन्दमय महत् अनुभव को प्राप्त कर लेता है। यदि यही क्रम है तो सब योग बाह्य रूप में चाहे कितने भी भिन्न दिखायी दें, इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं।
अब हमें यह विचार करना है कि विभिन्न योग वास्तव में मूल-प्रक्रिया पर किस भाँति कार्य करते हैं और क्या विधि अपनाते हैं? हम देखते हैं कि मनुष्य स्वयं को वाणी और कर्म द्वारा व्यक्त करता है। कोई भी मनुष्य चाहे वह अच्छा है या बुरा, उसका जीवन भी चाहे कैसा ही हो, उसकी वाणी और कर्म द्वारा पता चल जाता है। अशुद्ध एवं पाशवी प्रकृति का होने पर मनुष्य वीभत्स कार्य करता है। उसके सब कर्म अशुद्ध, कलुषित तथा हानिकारक होते हैं। वह औरों के प्रति दुःखदायी, कष्टकारक तथा विध्वंसक बन जाता है। जनता को वह अपमानित और दुःखी करता है। इस प्रकार कठोर, दुष्ट तथा बुरे वचन एवं कर्म मनुष्य की आसुरी प्रकृति के दर्पण-स्वरूप हैं। कर्म और वाणी द्वारा ही उसकी मनुष्यता प्रकाशित होती है, परन्तु योगियों तथा ऋषियों ने मानव के कर्म तथा वाणी से परे पहुँचने के यत्न किये। उन्होंने कहा : 'हमारे अन्तर्मन की गहराई में जो कुछ भी है, वाणी और कर्म उसको प्रकट करते हैं, अतएव सर्वप्रथम हमें यह प्रतीति होनी चाहिए कि इसका उद्गम कहाँ है?'
वाणी और कर्म का स्रोत जानने का प्रयत्न करते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि इनका मूल विचारों में ही समाया हुआ है। मनुष्य जो-कुछ भी सोचता अथवा मन में भाव लाता है, वह बाद में वाणी और कर्म के रूप में स्फुटित हो जाता है। बाह्य संसार में वाणी और कर्म यद्यपि अति-महत्त्वपूर्ण हैं, पर वे मनुष्य के बाह्य क्षेत्र पर महाविनाशकारी अथवा अद्भुत कल्याणकारी प्रभाव डालते हैं। वे और कुछ नहीं, केवल अन्तः शक्ति की बाह्य अभिव्यक्ति ही हैं, और यह शक्ति विचार-शक्ति ही है। सम्पूर्ण ज्ञान और ध्यान का अभिनिवेश करने के उपरान्त महापुरुषों को मालूम हुआ कि मन में रहस्यपूर्ण एवं जटिल तत्त्व हैं जिनका उन्हें सामना करना है। अतः मानव-मन का अध्ययन योग का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है।
मानव-मन का विश्लेषण, मानव-सत्ता के विभिन्न रूपों का सूक्ष्म अन्वेषण, मन किस प्रकार कार्य करता है, इसके विभिन्न भाव क्या-क्या हैं, इसके अनिवार्य रचना-तत्त्व (घटक) क्या हैं—यह सब योग का विषय है। (मन का) सोचना और उन (विचारों) का स्फुटित होना कई बातों पर निर्भर करता है। कर्म तथा वाणी की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। 'ऐसा क्यों है कि मन में एक विशेष प्रकार के ही भाव आते हैं? वह कौन-सा पदार्थ है जो विचारों का प्रतिपालन करता है?' उन्होंने अन्तर की गहराइयों में खोज की और अद्भुत अन्वेषण किये। वे क्या अन्वेषण थे? उन्हें ज्ञान हुआ कि विचार सर्वथा असम्बन्धित नहीं हैं। आपके समक्ष कुछ अत्यन्त सरल उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ जिनसे आपको मन के उस धर्म का सन्दर्शन होगा जो मानसिक जगत् में क्रियाशील है। वह धर्म क्या है?
दृष्टान्त-रूप से डाक्टर को देखने पर डिस्पेंसरी, अस्पताल और औषधि का ध्यान तुरन्त आ जाता है। यदि आप किसी सैनिक को सैनिक-वेष में देखें तो आपके मन में युद्ध, टैंक, बन्दूक तथा सैनिक आक्रमण के विचार आयेंगे। वकील को देखने पर आप न्यायालय, न्यायाधीश, दण्ड अथवा कारागार के सम्बन्ध में सोचेंगे।
इस प्रक्रिया में दो बातें समाविष्ट हैं। प्रथम, हमें एक नियम ज्ञात हुआ है कि पंचेन्द्रियों में से किसी के द्वारा भी यदि किसी विषय का ज्ञान होता है तो तुरन्त ही एक ऐसा विचार-क्रम बन जाता है जो अनुभूत विषय के समान ही होता है। यह साहचर्य का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार विचार के निर्माणार्थ यह आवश्यक नहीं कि विषय आपके नेत्र के सामने ही हो। आप स्मृति से कुछ सोचते हैं। स्मृति से जिस विषय का ध्यान किया, उसके सहकारी विचारों का क्रम तत्काल ही गतिशील हो जाता है। अतः ज्ञानी जनों ने यह खोज की कि मन की गहराई में विचारधारा को आदेश देने वाला साहचर्य-नियम ही क्रियाशील है।
एक और मनोरंजक नियम का भी आविष्कार हुआ। उन्हें पता लगा कि मन का एक विशेष अथवा दूसरे शब्दों में एक भयावह, गर्हित तथा कुत्सित स्वभाव है। साधकों के लिए यह एक सिरदर्द है। मनुष्य जो-कुछ इन्द्रिय-सम्पर्क स्थापित करता है, उसका विद्युत्-गति से अभिलेख रखना मन की बुरी आदत है। चलते हुए आप कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं अथवा कुछ अनुभव करते हैं, तत्काल ही विद्युत्-गति से अभिलेख एक संस्कार छोड़ जाते हैं। योगियों के लिए मन का महत्व संस्कार के विचित्र वैशिष्टय के कारण है। संस्कार चित्रपट पर खिंची हुई निर्जीव रेखा ही नहीं; अपितु सजीव लेखन है। अब आपको सजीव लेखन का आशय बताता हूँ। एक आलोकलेखा (Photographic record) होता है। कोई भी पदार्थ जो सूक्ष्मग्राही प्लेट पर आता है, तत्काल ही उस पर एक प्रतिकृति अंकित कर देता है जो सदा-सदा के लिए विद्यमान रहती है। जो आकृति आलोकलेखा-पटल ने अपने ऊपर बनायी है, वह आप से बात नहीं कर सकती; लेकिन संस्कार मन पर पड़ी हुई एक छाप है जिसमें व्यक्ति द्वारा किये गये उस वास्तविक अनुभव को पुनः सृजन करने की क्षमता है जिससे वह छाप बनी। संस्कार के स्वभाव का यह एक महत्त्वपूर्ण रूप है जो किसी भी अवसर पर सम्पर्क, व्यवहार अथवा अनुभव द्वारा (जो मनुष्य ने किये हैं) मन में रह जाता है।
संस्कार में यह क्षमता है कि मूलतः वह जिस भी अनुभव से बना है उसे पुनः ज्यों-का-त्यों प्रस्तुत कर सके। अपने बाह्य जीवन के एक अनुरूप उदाहरण द्वारा आप इसे भली-भाँति समझ सकेंगे। एक विशाल वृक्ष से हम फल-रूप एक छोटा-सा बीज प्राप्त करते हैं। वृक्ष बहुत बड़ा है और बीज बहुत छोटा; परन्तु इतना छोटा दिखने पर भी बीज की महान् क्षमता क्या है? जिस वृक्ष से यह (बीज) हुआ है, उसे फिर से पूर्ण विस्तार सहित उत्पन्न करने की इसमें पूर्ण क्षमता है। बढ़ने एवं शक्ति-सम्पन्न होने के लिए अनुकूल दशा एवं वातावरण मिलने पर यह छोटा-सा बीज उस वृक्ष को-जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है-सम्पूर्णतया पुनः अस्तित्व में ला सकता है। यही बात संस्कार के सम्बन्ध में भी है।
अनुमान कीजिए, आपको कोई पदार्थ चखने को दिया जाता है। वास्तविक रूप में स्वाद-क्षमता तो जिह्वा के दो-तीन इंच के क्षेत्र तक ही सीमित होती है। जिह्वा के सम्पर्क में आने से पूर्व स्वाद नहीं होता। जितने समय के लिए पदार्थ आपकी जिह्वा पर रहता है, उतने समय तक ही आप उसके स्वाद का अनुभव करते हैं। तथापि यह छोटा-सा अनुभव तत्काल ही संस्कार-रूप में मन में रख लिया जाता है। मान लीजिए, आप उस शहर अथवा नगर में जाते हैं जहाँ दश वर्ष पूर्व आपको उस पदार्थ का स्वाद लेने का अवसर मिला था तो आपको स्मरण हो आता १९४५ में मैंने यह पदार्थ खाया और उस विशेष स्थान पर खाया था।' आप कहीं बैठे हैं, उसका विचार करते हैं और कल्पना करने लगते हैं, वह (पदार्थ) कितना रुचिकर था और कैसे आपके मुख में जाते ही घुल गया। इससे संवेदन-प्रतिक्रिया आरम्भ होती है और कल्पना तुरन्त संस्कार को इच्छा के रूप में परिवर्तित देती है।
प्रथमतः संस्कार वासना के रूप में रहता है। वासना वृत्ति का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार मानसिक प्रक्रिया आरम्भ होती है। कल्पना-शक्ति द्वारा पुनः सृजन का क्रम इच्छा के रूप में स्फुटित होता है। और एक बार इच्छा उत्पन्न हुई नहीं कि मनुष्य उसे पूर्ण करने के यत्न में लग जाता है। वह उस इच्छा का दास बन जाता है। इच्छा होने पर उसे पूर्ण करने का यत्न करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक ही है। शीघ्र ही अह भी कहता है- 'मुझे तो यह प्राप्त करना ही है।' अहं-भाव इच्छा से तादात्म्य कर लेता है; परन्तु यदि अहं-भाव में उच्चतर विवेक हो तो वह इच्छा के साथ समरूप होने की अपेक्षा उच्च विवेकशील तत्त्व बुद्धि से समरूप होने का प्रयास करता है जो कहती है- 'मुझे यह नहीं चाहिए।' परन्तु साधारणतया अहं-भाव में विवेक की क्षमता नहीं होती और यह अपने को इच्छा का ही स्वरूप बना कर विभिन्न इन्द्रियों को आदेश देता है। आप टेलीफोन की डायरेक्टरी देखते हैं और उस दुकान का नम्बर खोजते हैं जहाँ से आष अपनी इच्छित वस्तुएँ खरीद सकते हैं। यदि आपको नम्बर मिल जाता है तो आप उसी समय फोन पर ही आर्डर दे देते हैं। यदि आपको नम्बर नहीं मिलता तो आप टैक्सी ले कर उस दुकान तक पहुँचते हैं, खाद्य पदार्थ लाने के लिए आज्ञा देते हैं एवं उसका स्वाद लेते हैं। अनुभव पुनः सृजित हो जाता है। यह अनुभव एक नवीन संस्कार बनाता है अथवा पूर्व-संस्कार को गहरा कर देता है।
संस्कार में बहुत शक्ति होती है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए जिससे आप नया संस्कार ग्रहण न कर सकें। योग-प्रक्रिया संस्कारों को इस प्रकार नष्ट करने की अपेक्षा रखती है कि उनका पुनर्जन्म न हो-जैसे आप एक बीज को तवे पर रख कर भून लें और फिर उसे भूमि में बोयें तो वह अंकुरित नहीं होगा; क्योंकि उसका जीवन-तत्त्व पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है। ऐसा ही समाधि की अवस्था में होता है जिसमें सब संस्कार नष्ट कर दिये जाते हैं। संस्कार तो अनगिनत हैं; परन्तु यहाँ मैं केवल एक ही संस्कार का वर्णन कर रहा हूँ, जो बहुत शक्तिशाली है। अपने जाने-अनजाने में हम प्रतिदिन, प्रातः से ले कर सायंकाल पर्यन्त ऐन्द्रिक (इन्द्रिय-सम्बन्धी) अनुभवों का संचय करते हैं। हम प्रतिदिन जो-कुछ भी अनुभव करते हैं, वह संस्कार का रूप धारण कर लेता है। जीवन के प्रत्येक जाग्रत-क्षण में हम संस्कार एकत्र करते रहते हैं। अतएव मनीषी गण कहते हैं कि एक-एक करके सब संस्कारों को समाप्त करना असम्भव है। अणुबम के गिरने से जिस प्रकार एक-साथ सहस्रों लोग मारे जाते हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा दिये हुए अस्त्र समाधि अर्थात् परम चैतन्य की अनुभूति द्वारा सदा-सदा के लिए सब संस्कार नष्ट हो जाते हैं जिससे कि उन्हीं संस्कारों को उत्पन्न करने वाले अनुभव फिर न हो सकें। गहन ध्यान द्वारा योगी संस्कारों को नष्ट करते हैं और संस्कारों को नष्ट करने से मनुष्य बन्धनमुक्त हो जाता है। योग का यही मार्ग है। पूर्व-काल के योगियों तथा ऋषियों ने मन के विषय में जो-जो खोजें कीं, उनमें से यह एक है। राजयोग के सम्बन्ध में कहा जा सकता है-मन के संस्कारों को विनष्ट करने की विधि।
हमें कुछ और सामान्य तत्त्वों का सन्दर्शन करना है जो मन से सम्बन्धित हैं। हमें ज्ञात करना है कि इस अद्भुत माया-जाल में उनकी भूमिका क्या है। हमें देखना है कि सीमित व्यक्तित्व में मन आत्म-चेतना तथा विचार-प्रक्रिया को किस प्रकार पकड़े रखता है, कैसे कार्य करता है तथा कैसे घनीभूत बनता है। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। हमें यह प्रतीत होना चाहिए कि विचार मनुष्य के अन्तःकरण से ही सम्बन्ध रख कर केवल मन को ही प्रभावित नहीं करते, प्रत्युत् मनुष्य के बाह्य जीवन के सब क्षेत्रों में उनका शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है; उसके प्रत्येक कर्म-क्षेत्र से उसके व्यक्तित्व का सुस्पष्ट एवं ठोस भाग बन जाते हैं। इतना ही नहीं, निर्बन्धित किसी विशेष अवस्था अथवा निश्चित अनुभवों की भाँति उनमें विषयपरक बाह्य स्वरूप बनने की शक्ति भी है। अतः विचारों के प्रति हमें अवश्यमेव सावधान रहना चाहिए।
हमें मालूम होना चाहिए-क्या सोचना है और कैसे सोचना है। हमें चाहे यह मालूम हो कि क्या सोचना अच्छा है; परन्तु हम उस विचार को ग्रहण नहीं कर पाते और अन्य कोई विचार, जिसका चिन्तन हम नहीं करना चाहते, क्रियाशील हो कर हमारे चेतना-पटल पर अधिकार कर लेता है। जिन लोगों को अभी तक यह अनुभव नहीं हुआ कि उनका अस्तित्व उनके विचारों से सर्वथा भिन्न है, ऐसे लोगों के लिए यह सामान्य अनुभव एवं प्राकृतिक नियम है। यदि वे चाहें तो स्वामी बन कर अपने विचारों को किसी भी दिशा में स्वयं प्रेरित कर सकते हैं। मनुष्य को इस सत्य का ज्ञान होना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि 'मैं एक चीज हूँ और विचार सर्वथा दूसरी चीज है जो मेरे मूल-स्वभाव का अंग नहीं है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसको मैं संचालित कर सकता हूँ। यह आवश्यक नहीं कि वह ही मेरा मार्ग-दर्शन करता रहे।' इस सत्य के सम्बन्ध में जब तक व्यक्ति सावधान नहीं हो पाता तब तक वह विचारों का दास बना रहता है। उस समय आप विचारों को प्रेरित नहीं कर रहे; अपितु विचार आपको प्रेरित कर रहे हैं। अतः हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि विचार हमारे अन्दर किस भाँति क्रियाशील होते हैं और हमारे बाह्य जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है।
तृतीय विषय है साधना का ऐक्य। हम ज्ञात कर चुके हैं कि मनुष्य के अधम, स्थूल एवं पाशविक प्रकृति में बन्धन का मूल-कारण उसके कुविचार हैं। यह वे विचार हैं जो अपने स्वत्व को निम्न प्रकृति की ओर साग्रह प्रवृत्त करते हैं और हम जानते हैं कि विचार जो इच्छा, क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या एवं मोह जैसे प्रमुख दुर्गुणों पर आधारित हैं, किस प्रकार मनुष्य को स्वभावतः अधम बनाये रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने विचार की गहराई में पहुँच कर ज्ञात किया है कि योग का प्रथम कार्य विचारों को वश में करना एवं मनुष्य की प्रकृति में पूर्णतया परिवर्तन लाना है। यदि मन का रुझान निम्न तत्त्व की ओर है तो वह चेतना को ऊपर नहीं उठा सकता; परन्तु यदि उसकी निष्ठा आत्म-तत्त्व में है तो वह उसे निम्न से उच्च, सूक्ष्म, आध्यात्मिक स्तर तक ले जाने का एक प्रभावपूर्ण उपयुक्त साधन और माध्यम बन सकता है। अतएव, उन्होंने मन और मन के रहस्यों को जानने हेतु प्रयत्न किया।
मन का रूपान्तर ही योग का प्रथम उद्देश्य है। हमें विदित है कि रूपान्तर यदि अपवित्र से पवित्र, सान्त से अनन्त एवं स्थूल से सूक्ष्म और अध्यात्म की ओर को हो तो सारभूत रूप में सब योग-विधियाँ एक प्रकार से ही (क्रियाशील) होंगी। अतएव अब हम देखेंगे कि साधना का ऐक्य चारों योगों में किस भाँति विद्यमान है, जो बाह्यतः भिन्न दिखायी देते हैं।
वेदान्त-मत के अनुसार जीव के अस्तित्व का मूल-कारण अज्ञान अथवा मूलाविद्या है। मूलाविद्या का प्रथम रूप परम चैतन्य, अद्वैत में द्वैत का भान करना है। तदुपरान्त अविद्या के कारण विचार उत्पन्न होता है कि मैं संसार से भिन्न हूँ। द्वैत-भाव के कारण अध्यास उत्पन्न होता है।
चैतन्य-तत्त्व अनन्त विश्व-रूप (प्रभु) से तादात्म्य करने की अपेक्षा व्यक्तिगत सान्त शरीर से अनन्य मान लेता है। यह अविद्या की प्रथम अभिव्यक्ति है। 'मैं यह शरीर हूँ', 'मैं यह मन हूँ', 'मैं यह भाव हूँ', 'मैं यह विचार हूँ- यह सब तादात्म्यता के क्रम हैं जो प्रथम भ्रम 'मैं एक भिन्न पदार्थ हूँ' में बद्धमूल हैं। द्वैत-भाव प्रथम मिथ्या अध्यास का क्रम आरम्भ करता है और इसी कारण अध्यास का भ्रम होने लगता है। हम शुद्ध आत्म-तत्त्व पर विभिन्न रूपों एवं गुणों, जो कि उसकी मूल-प्रकृति के रूपों में वहाँ नहीं हैं, का अध्यास (आरोपण) करते हैं। इसी कारण सम्पूर्ण जगत् का दृश्य-प्रपंच आविर्भूत होता है।
सर्वप्रथम अज्ञान है। उस अज्ञानता के कारण ही द्वैत-भाव उत्पन्न होता है, तदनन्तर शरीर और मन आदि के संग अध्यास। यह अज्ञान मन के अशुद्ध विचारों पर ही आधारित है और इसीलिए इस क्रम में परिवर्तन लाने हेतु शुद्ध विचार लाने का क्रम आरम्भ किया जाता है। स्वामी विवेकानन्द ने इसे आधुनिक सम्मोहन कहा है। उन्होंने कहा है कि स्वयं को शरीर समझ कर आत्म-तत्त्व ने अपने को मिथ्या विचारों के वशीभूत कर दिया है। आपको इस सम्मोहन से जागना है। उन्होंने कहा है कि उचित विचारों एवं विवेक के कारण वेदान्त इस कृत्रिम निद्रा (सम्मोहन) का विनाशक है। आपको जागरूक हो जाना चाहिए और यही उचित विधि है। सम्पूर्ण वेदान्त-साधना शुद्ध विचार पर आधारित है। चिन्तन के लिए आपमें सही विवेकशीलता का होना अत्यावश्यक है। सर्वप्रथम तो आपको ज्ञात करना है कि सत्य क्या है? तभी आप सत्य की ओर ले जाने वाले तत्त्वों का चिन्तन कर सकते हैं। अतः सबसे पहले उन्होंने परम सत्य के सम्बन्ध में श्रवण का निर्देशन दिया। जैसा कि आप जानते हैं, यह भी वेदान्त का एक अंग है।
आपको विवेकशीलता के द्वारा शुद्ध विचार-प्रवाह को बनाये रखना है। विचार-प्रवाह को परम सत्य की ओर अग्रसर करने के लिए वेदान्त एक रूप-रेखा प्रस्तुत करता है। आप इस वास्तविक कार्य को मनन में करते हैं और मनन की पराकाष्ठा ही ध्यान है। चैतन्य की विविध मानसेतर समाधि नामक अवस्थाएँ हैं। समाधि में भी सवितर्क, निर्वितर्क आदि कई अवस्थाएँ हैं। जब मन की सब क्रियाएँ समाप्त हो जाती हैं, उसे अद्वैत या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उस अवस्था में मनुष्य सदा के लिए अज्ञान के बन्धन से मुक्त हो जाता है। मन के निष्क्रिय होने पर कोई भी अनुचित अनुभव नहीं हो सकता। यह वेदान्तिक साधना की आन्तरिक प्रक्रिया है। तब आप स्वयं को इस शरीर के साथ एकरूप (देहाध्यास) करने की अपेक्षा अनन्त, निराकार, परम सत्ता के साथ तादात्म्य कर लेते हैं।
परन्तु यह विचार अन्य रूपों में भी प्रकट होता है। भाव-रूप में प्रस्फुटित होने पर विचार अनेक प्रकार के स्वयं अपने और अपने प्रियजनों के प्रति मोह एवं प्रेम-प्यार जैसी मिथ्या आसक्ति को प्रकट करता है। मोह चैतन्य-तत्त्व को अनुचित भाव और संवेगों की सीमा में बाँध देता है। मोह से ममता अर्थात् 'यह घर मेरा है', 'बच्चा मेरा है' अथवा 'सम्पत्ति मेरी है' आदि भाव उत्पन्न होते हैं। अतः तत्त्वज्ञानियों ने मन के मिथ्या संवेगों अथवा
बन्धनों और मिथ्या आसक्तियों के इस अयथार्थ प्रकटीकरण का सामना करने के लिए एक और विधि का विकास किया है। वह है विराग और राग की विधि-सांसारिक विषयों से अपने व्यक्तित्व के सम्पूर्ण संवेगात्मक पक्ष को अलग कर देना तथा किसी पूर्ण एवं दिव्य व्यक्तित्व के प्रति अनुरक्त होना। भक्ति और इष्ट की संकल्पना इसी पर आधारित है।
संसार की नश्वर वस्तुओं के प्रति भावुक बन कर मोह रखने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना चाहिए; वैराग्य प्राप्त करके अपनी सम्पूर्ण सांवेगिक शक्ति को किसी पूर्ण दिव्य व्यक्तित्व के प्रेम में लगा देना चाहिए। यह मन को बाह्य विषयों से शनैः-शनैः विरक्त करना तथा सर्वव्यापक दिव्य तत्त्व में इसे एकाग्र करना भी मन एवं भावों की शुद्धि का ही एक अन्य क्रम है। कोई भी दैविक शक्ति, जिसको भक्त आराधना हेतु चुनता है, इष्टदेवता कही जाती है।
ईसाई-मत के समान जिनके समक्ष केवल एक ही आदर्श है, वे परम सत्य के अनेक रूपों में विश्वास नहीं रखते। ईसाइयों के समक्ष केवल एक ही रूप है-स्वर्ग में निवास करने वाले प्रभु पिता (Father in heaven)। अधिकतर ईसाई भक्त हैं। वे प्रभु-प्रेमी होते हैं। जिनका एक ही इष्टदेवता होता है, उनमें भी मानुषिक प्रकृति का असंयमित आग्रह पाया जाता है। वे ईसा मसीह को सर्वसम्पन्न वर की भाँति प्यार करना चाहते हैं, कुछ तो 'क्रास' पर चढ़े ईसा की ही आराधना करते हैं और वही दुःख भोगना पसन्द करते हैं, जो ईसा ने सहन किये। कुछ और लोग प्रौढ़ ईसा को पूजने की अपेक्षा उन्हें 'मेरी' की बाँहों में (देख कर) प्रेम करते हैं। उनमें से कुछ गुरु-रूप में शिष्यों के साथ रहने और घूमने वाले ईसा के रूप को चाहते हैं। अतएव, अपनी-अपनी प्रकृति एवं रुचि के अनुसार एक ही धर्म में एक ही इष्टदेवता के विभिन्न रूप भक्तों को आकर्षित करते हैं।
उसी प्रकार, मनुष्यों को निम्न से उच्च स्तर तक लाने के अभिप्राय से हिन्दू-धर्म ने अनेक अवतार, भाव एवं मनोवृत्तियाँ प्रस्तुत की हैं। अभी तो हम पूर्णरूपेण मन की भावुकता पर प्रकाश डाल रहे हैं और इसीलिए बुद्धिमानों ने अन्यान्य भाव दिये हैं जिनसे व्यक्ति-विशेष के प्रति मोह को सर्वातिशायी ईश्वर के मोह में अनायास ही रूपायित किया जा सके। यदि प्रभु से आपका प्यार ऐसा है जैसा कि माँ का बच्चे से होता है तो यह वात्सल्य कहलायेगा। इसके अतिरिक्त और भाव भी हैं। सख्य-भाव में आप प्रभु से अपने मित्र की भाँति प्रेम करते हैं। अर्जुन के अन्दर यही भाव था और उद्धव ने भी ऐसा ही प्रेम किया। इसके अतिरिक्त साधारण व्यक्ति और भक्त सेवक का प्रेम अर्थात् उनका सेवक-स्वामी-भाव भी एक दिव्य आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। मन के भाव और चिन्तन के क्षेत्र में सर्व प्रकार के प्रेम भक्ति-योग द्वारा दिव्य प्रेम में परिवर्तित किये जा सकते हैं।
एक और भी बात है। मन की अनेक विषय-ग्रन्थियाँ भी हैं। भिन्न-भिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न ग्रन्थियाँ हैं जो विभिन्न पदार्थों के संसर्ग से बनती हैं। अनुमान कीजिए कि आपका शरीर सुन्दर है। आपके अन्दर भाव उठता है- 'मैं अतीव सुन्दर हूँ और आपमें उत्कर्ष (श्रेष्ठता) का भाव उत्पन्न होता है। यदि आपके पास धन है तो आप सोचते हैं- 'मैं समृद्ध हूँ' और आप ऐसे लोगों को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं जिनके पास धन नहीं है। यदि आपके पास बहुत-सी जानकारी है अथवा आप प्राध्यापक हैं तब भी श्रेष्ठता की भावना-रूप से अहंभाव आपके मन में आता है और सोचते हैं कि आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। आप संगीत में निपुण हैं या मुक्केबाजी जानते हैं-कुछ भी ज्ञान आपमें हो, तुरन्त वह (ज्ञान) अभिमान में रूपायित हो जाता है। आपमें वंश, धन-दौलत (समृद्धि), ज्ञान, शक्ति, सौन्दर्य, प्रतिष्ठा, उच्च-पद आदि की श्रेष्ठता की भावना हो सकती है। ये सब अभिमान कही जाती हैं। इन सब विषमताओं का शरीर से सीधा सम्बन्ध होने के कारण जीव के लिए यह बन्धन अत्यन्त विकट है। अतः अहं के बन्धन से आप छुटकारा नहीं पा सकते।
वेदान्त का गूढ़ ज्ञान देह-भाव को समूल नष्ट कर देता है; परन्तु जो वेदान्त का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और अभिमान के जाल में ही फँसे हैं, उनको अहं की संज्ञा पाने वाली सभी भावनाओं को कुचलना होगा।
परन्तु कैसे ? नितान्त विनम्र बन कर । सब तुच्छ भावों का त्याग कर, जो सामान्यतर, सरलतम और विनम्रतापूर्ण है, उसके साथ एक हो जाओ। स्वयं को अति सामान्यता, सरलता एवं नम्रता के स्तर पर लाना ही अभिमान का त्याग करना है। कर्मयोग की अद्भुत कला द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। एक कर्मयोगी को दूसरों से काम नहीं लेना चाहिए। उसे अपने कपड़े स्वयं धोने चाहिए और अपना कमरा स्वयं साफ करना चाहिए। उसे भार उठाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। स्वयं को नगण्य समझना चाहिए। अभिमान को दूर करने के लिए आपको वे कार्य करने चाहिए जो कि एक अधः मन करना पसन्द नहीं करता। अतः कर्मयोग अभिमान के विरुद्ध संघर्ष का उद्घोष है। कोई स्त्री यदि गठरी नहीं उठा सकती तो कर्मयोगी तुरन्त जा कर उसकी गठरी स्वयं उठायेगा। एक साधारण व्यक्ति अभिमानवश ऐसा नहीं करेगा। वह किसी को पहले नमस्कार नहीं करेगा। अभिमान को निरन्तर मिटाते रहिए।
गान्धी जी एक महान् कर्मयोगी थे। उनका कहना था कि वर्धा जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले तीन मास तक शौचालय साफ करने का कार्य करना पड़ता था। भारत में सबसे निम्न कर्म यही शौचालय साफ करना समझा जाता है और वे ही लोग अछूत माने जाते हैं जो यह कार्य करते हैं। उन्हें छू लेने पर स्नान करना आवश्यक समझते हैं। अमरीका तक में लोग समाज के निम्न-वर्ग से सम्पर्क नहीं रखते। उनके बीच सामाजिक स्तर एवं सम्पत्ति विघ्न-स्वरूप है। इंगलैण्ड में भी यह भावना बहुत कुछ ऐसी ही है। आप ऐसा कार्य करें जिससे कि आप सोचते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुँचती है। स्वयं को शून्य बनाने के लिए श्रेष्ठता की भावना को सर्वथा दूर कीजिए। इससे आपमें सादगी, नम्रता और साधुत्व की भावना जागृत होगी और आपका हृदय विशाल बनेगा। सब वर्ग के लोगों को आप आत्म-स्वरूप ही समझने लगेंगे। इससे चैतन्य-तत्त्व को भी उच्चतर अवस्था में ले जाने के हेतु आप भूमि तैयार करते हैं। शुद्ध मन में दिव्य सात्त्विक विचार ही आयेंगे। कुछ लोगों की दृष्टि में कर्मयोग एक स्वतन्त्र योग-पद्धति है, जब कि अन्य दूसरे व्यक्ति इसे सहकारी-योग मानते हैं।
राजयोग में पतंजलि ऋषि ने कहा है कि आपको विचार द्वारा ही अज्ञान का प्रतिरोध करना है। निःस्वार्थ सेवा अथवा कर्मयोग द्वारा स्वयं को पूर्णतया नम्र बना कर आप अपनी गहराई तक पहुँची हुई प्रत्येक ग्रन्थि को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न करें। निम्न वर्ग उच्च-वर्ग की सेवा करने के लिए माना गया है। अतः आप निम्न-मनुष्य के करने योग्य कर्म तथा सरल, समर्पण और निःस्वार्थ भाव से सेवा करें। ईसा मसीह ने इसे अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया। रात्रि के अन्तिम भोजन से पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों के चरण धोये। पतंजलि ने भी कहा है: “मन को मिथ्या एवं नश्वर विषयों से मोह है; अतः इस दुष्ट को क्यों न निरुद्ध कर दिया जाये?" हमें इसे पूर्ण रूप से निष्क्रिय करना है। फिर वह क्या कर सकता है? इसलिए मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। मन की सब विचित्र कल्पनाएँ रुक जायेंगी।
वृत्ति-निरोध
विचार-प्रवाह की जड़ें मानसिक क्रियाओं में निहित हैं। मन के क्रियाशील होने के कारण ही विचार, भाव एवं प्रत्येक प्रकार का मिथ्या प्रत्यक्ष बोध स्फुटित होता है, इसलिए मन की क्रियाओं को निश्चल कीजिए। क्रियाशील मन की प्रथम अभिव्यक्ति के बारे में वर्णन दिया जा चुका है। मन के सरोवर में एक तरंग उठती है। इसके पश्चात् कल्पना का आगमन होता है और फिर इच्छा का। इन सबसे पूर्व तो केवल विचार ही उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से रहित यह शुद्ध चिन्तन ही मनस्तत्त्व पर प्रक्षेपित होता है। कल्पना और स्वाभिमान विचार के साथ जुड़ने पर ही पूर्ण क्रम स्फुटित होता है। केवल विचार में कोई शक्ति नहीं होती। यदि आप इसके साथ मिल जायेंगे तो यह एक प्रभावशाली दुष्ट कार्य करने वाला बन जायेगा। बुद्धिमानों ने कहा है: "सब विचारों का पूर्ण रूप से निरोध कर दें। मन-रूपी सरोवर में एक तरंग भी न उठने दें। इसे सर्वथा शान्त कर दें। कोई भी वृत्ति नहीं रहनी चाहिए। मन की मूल अभिव्यक्ति को ही प्रशान्त कर दें।" महर्षि पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट प्रथम सूत्र ही यही है- "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" अर्थात् चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है।
जब मन की क्रियाएँ सर्वथा शान्त हो जाती हैं तो परम चैतन्य का उदय होता है। परम चैतन्य के प्रादुर्भाव के लिए अनुकूल स्थिति मन के सर्वथा निरुद्ध होने पर होती है। अतः समाधि में परम चैतन्य के उदित होने पर सब वासनाएँ निर्मूल हो जाती हैं। जैसे प्रत्येक बीज में एक वृक्ष बनने की सम्भावना निहित है; परन्तु यदि आप बीज को भून लें और फिर अच्छी भूमि में डाल कर पानी दें तो वह अंकुरित नहीं होगा। योग के अनुसार ज्ञानाग्नि में वासनाएँ जल जाती हैं। महर्षि पतंजलि ने अध्यास के मूल को ही पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि इस उपद्रवी मन को सदा के लिए रोक लीजिए। राजयोग में मन की क्रियाओं को निष्क्रिय करने का उपाय बताया गया है। अतः आप देखते हैं कि सब योगों का मूल प्रयास मन के विभिन्न पक्षों को वश में करने की ओर है, उन विविध पक्षों को जो जीवात्मा को निम्न आत्मा से जकड़े हुए हैं। और इन विविध पक्षों में से जिस व्यक्ति के लिए मन का जो पक्ष अनुकूल होता है, वही पक्ष उसमें प्रधानता पा लेता है। स्वामी शिवानन्द जी ने कहा है- "आपको एकांगी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। यदि आप राजयोग के अनुसार चलते हैं तो और योग भी आपको सहकारी रूप में करने चाहिए।" स्वामी जी योग-समन्वय को महत्त्व देते थे। आपमें भक्तियोग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोगादि सब योगों का संयोग होना चाहिए। साधना का यह ऐक्य अत्यन्त हितकारी है। सभी योग अज्ञानावस्था के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न अध्यास, अयथार्थ कार्यशीलता एवं भाव को उच्चावस्था में लाने के हेतु मन के रूपान्तर के उसी क्रम की ओर प्रेरित करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में किसी एक ही रूप के प्राबल्य के कारण सबके मार्ग अलग-अलग हैं।
कोई भी विचार, जो मन में स्थायी हो जाता है, प्रबल होने लगता है और मन में स्वयं को दोहराने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। आप कुछ भी चिन्तन करें, उसे पुनः-पुनः सोचना मन की स्वाभाविक प्रकृति है। मन में जो विचार जानबूझ कर स्वीकृत हुआ है, वह तुरन्त ही अपनी पुनरावृत्ति चाहता है और जो कुछ भी आप सोचते हैं, वह कर्म के रूप में व्यक्त हो जाता है। यदि आपमें दयाभाव उठता है तो आप दयाभावयुक्त कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। यदि आप विषय-परायण अथवा लोलुप विचारों में संलग्न हैं तो हठात् ही कर्म भी आप ऐसा करेंगे जो विषयपरक अथवा लोलुप होगा। क्रोधित भाव आपको कठोर कृत्य करने को बाध्य करता है और कामुक भाव ऐसा कर्म करने के लिए प्रेरित करता है जिसमें राग की झलक हो। कोई भी विचार मनुष्य को अपने अनुरूप कार्य करने को प्रेरित करता है। यह दूसरी बात है जिसे आपको समझना है।
कर्म की यह प्रकृति है कि एक बार होने पर यह पुनरावृत्ति चाहता है और पुनः-पुनः करने पर कर्म मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। अनजाने में ही आप उस विशेष प्रकार के कार्य के अनुगामी बन जाते हैं। आदत तृतीय स्थिति है, जो एक विशेष प्रकार के विचार को दृढ़ करने से बनती है। आपकी आदतों से आपका चरित्र प्रभावित होता है। चरित्र भाग्य का विधायक है। इस प्रकार विचारों से कर्म, कर्म से स्वभाव, स्वभाव से चरित्र एवं चरित्र से भाग्य का उदय होता है। अब, युक्त विचारों के महत्त्व की प्रतीति आपको हो गयी होगी। आप सावधानी से उन सब विचारों को दूर करें जो आत्मिक उन्नति अथवा अन्तराभिव्यक्ति के प्रतिकूल हैं।
योग-साधना
आध्यात्मिक विकास में मन सबसे बड़ा शत्रु है। कामना, विक्षेप, चंचलता आदि विविध रूपों में मन ही विकटतम बाधा है। यदि मन पूर्णतः स्थिर हो तो आत्मा का प्रकाश स्वयं ही प्रतिबिम्बित होता है। अहंकार, तुच्छ स्वाभिमानी व्यक्तित्व हमें अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देखने देता। इसमें स्मृति भी महान् बाधा है। मन के उपर्लिखित रूपों सहित अविचार-बुद्धि आत्मघातक है। इससे आत्मिक चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। विचार की अप्रतिहत प्रवृत्ति कर्म में परिवर्तित होना है और प्रत्येक कर्म मानुषिक प्रकृति में आदत बन जाता है और जब व्यक्ति आदतों का शिकार हो जाता है तो आदत उसके स्वभाव का अविभाज्य अंग बन जाती है।
मनुष्य का समस्त व्यवहार उसके चरित्र पर आधारित है। बाद में प्रत्येक कर्म प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने वाला बीज-स्वरूप बन जाता है। जीवन-यापन करते हुए व्यक्ति कर्मों की संरचना करता है जो उसका भाग्य बन जाता है। अतः हम देखते हैं कि विचार किस प्रकार मनुष्य के भाग्य को शासित करते हैं और चुने हुए उत्कृष्ट विचारों के चिन्तन का क्या महत्त्व है तथा अयथार्थ चिन्तन से बचना क्यों आवश्यक है। राजयोग के विज्ञान का मुख्य उद्देश्य उन सब क्रियाओं को रोकना है, जो मन की मुख्य क्रियाएँ हैं; परन्तु हम तो पहले ही राग-द्वेष, कल्पना, विचार आदि इसकी फैली हुई सूक्ष्म शाखाओं के शिकंजे में हैं। इसलिए मूल तक पहुँचने के पूर्व ही हमें इसकी शाखाएँ नष्ट करनी हैं। यदि आप सिंह का सामना करना चाहते हैं तो पहले आपको वन में जाना पड़ेगा, उसके उपरान्त ही आप उसकी कन्दरा तक पहुँच सकेंगे। चित्तवृत्ति मन-रूपी सिंह की कन्दरा है। आपको इसकी ईर्ष्या-द्वेष, काम, घृणा आदि भावनाएँ नष्ट करनी हैं तथा असद् कर्मों की राशि का, जो बुरे विचारों से बनी है, शोधन करना है। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए यह आक्रमण-क्षेत्र को परिमित करने की प्रक्रिया है।
मानसिक क्रियाओं की दूर तक फैली हुई बाह्य अभिव्यक्तियों को नष्ट करने हेतु पतंजलि ऋषि ने राजयोग की अत्यन्त वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप में व्याख्या की है। मनुष्य एक विवेक-युक्त प्राणी है। उसमें अधम तत्त्व भी है, जो उसे नीचे की ओर ले जाने की चेष्टा करता है। उसकी एक तत्त्वतः आध्यात्मिक प्रकृति है और इन दोनों के मध्य में बुद्धि-युक्त मनुष्य है जिसके मन होने से सोचने की क्षमता है। अतः मध्य में चिन्तन-शक्ति-युक्त प्राणी है, जो मनुष्येतर कोटि के जीवों, जिनमें सोचने की शक्ति नहीं है, से भिन्न है।
मानव के सारभूत स्वभाव के अध्ययन के परिणाम के अतिरिक्त ऋषि पतंजलि ने उसकी वास्तविक रचना का भी अध्ययन किया और उपर्लिखित निष्कर्ष पर पहुँचे। उन्होंने किसी हिन्दू अथवा मुसलमान के नहीं; अपितु मनुष्य के सार्वलौकिक स्वरूप का अध्ययन किया जो सृष्टि के आदि में सर्वत्र रचा गया और जिसका रूप उसके अस्तित्व के अन्तिम दिन तक (वैसा ही) रहेगा। उन्होंने ज्ञात किया कि आरम्भ में तो वह नितान्त सत्ता मात्र होता है। तत्त्वतः वह आत्मा ही है। उसका अस्तित्व आध्यात्मिक है, यह प्रत्येक मानव को जिसमें सोचने की क्षमता है, ज्ञात है। मनुष्य का अन्तिम तत्त्व उसकी सत्ता ही है। कोई भी अपने निस्तत्त्व होने की कल्पना नहीं कर सकता; क्योंकि ऐसी कल्पना करने के लिए भी तो एक कल्पना करने वाले की आवश्यकता होगी, इसीलिए कल्पना करने वाला ही आत्यन्तिक सत्ता (ब्रह्म-स्वरूप) है। मनुष्य का अविनाशी तत्त्व उसकी आत्मा है। वह सत् है। मेरा अस्तित्व है, मैं सत् हूँ, शुद्ध ब्रह्म हूँ, केवल सत् हूँ। और मनुष्य में यह सार-भाग ही उसके अस्तित्व का मूल अंग है। पतंजलि ऋषि को ज्ञान हुआ कि मानव का मूल-तत्त्व तो अन्तर में ही कहीं है; पर एक-दूसरे को देखने पर उसकी भौतिक सत्ता दृष्टिगोचर होती है। हम मनुष्य की प्रतीति उसके विशेष रूप, आकार एवं अंगों से करते हैं। अतः ऋषि पतंजलि ने कहा-मनुष्य का शरीर स्थूल कोश है। यह मनुष्य का एक पक्ष है। उसमें एक और तत्त्व है जिसमें सोचने की शक्ति है। मानव-सत्ता का मानसिक स्वरूप भी होता है जिसे मनोमय कोश कहते हैं। चिन्तन-शक्ति का आविर्भाव होता है; विचार आते हैं और व्यक्ति सोचने लगता है। इन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए शरीर क्रियाशील होता है। मनुष्य का पूर्ण जीवन ही विचारों की भावाभिव्यंजना है और यह भावाभिव्यक्ति विविध कर्मों के रूप में होती है। अतः निश्चय ही भौतिक शरीर में विचारशील मनुष्य विद्यमान है। उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में एक सम्बन्ध-सूत्र है। चिन्तनशील एवं क्रियाशील मनुष्य के मध्य में एक शक्ति है जो कार्यशील है। विद्युत् के समान अदृश्य एवं आन्तरिक शक्ति है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए बाध्य करती है। शक्ति जो मानव को सजीव (चेतन) बनाती है, जिसके बिना सब इन्द्रियाँ नितान्त निष्क्रिय हो जाती हैं, वह प्राण-शक्ति है। चक्षु प्राण-शक्ति द्वारा देख सकते हैं। कर्ण प्राण-शक्ति द्वारा सुनते हैं। जिह्वा प्राण-शक्ति द्वारा ही बोलती है।
मृत्यु के समय प्राण निकल जाने पर विघटन-क्रम आरम्भ होता है। शरीर से प्राणों का उत्क्रमण ही मृत्यु है। वास्तव में हम सब चलते-फिरते तथा बोलते हुए शव हैं। प्राणों के प्रयाण कर जाने पर हम सर्वथा गतिहीन हो जाते हैं; क्योंकि प्राण ही शरीर को संचालित कर रहा है, वही कार्य कर रहा है, खा रहा है, आनन्द ले रहा है आदि। यह सब प्राण-शक्ति के कारण है। यह मानव का तृतीय स्वरूप है और इसके पीछे सबको चलाने वाली शुद्ध आत्मा है; 'अहं अस्मि' । परन्तु एक विचित्र-सा भ्रम हो जाता है, जिसके कारण आप स्वयं का मन से तादात्म्य कर लेते हैं और स्वयं को मन का ही एक अटूट अंग मानने लगते हैं; यद्यपि कभी-कभी अनजाने में आप अपने असंग साक्षी-स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं। जब आप कहते हैं-"मेरा मन अशान्त है", आप अनजाने में यह स्वीकार करते हैं कि आप मन से पृथक् हैं और मन नाम की कोई वस्तु आपके पास है। तो जब आप ऐसा कहते हैं कि 'मेरा मन अशान्त है' अथवा 'मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता' आदि, उस समय आप मन से पृथक् होते हैं। यह सब आपकी वास्तविक प्रकृति के स्वत:प्रेरित भाव हैं। अतः भौतिक शरीर-कोश, प्राण-कोश एवं मन-कोश-जीव के ये तीन रूप अल्पकालिक, क्षणिक, दिखावटी तथा अनावश्यक हैं। आवश्यक तत्त्व केवल आत्मा ही है। आपका स्वत्व शुद्ध-सत्ता है जो अजन्मा, शाश्वत एवं पुरातन है-"अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण: ।" मन के प्रकट होने से अति-पूर्व आपका अस्तित्व विद्यमान था। पतंजलिकृत मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का-शुद्ध आत्म-तत्त्व के केन्द्र का अध्ययन जो मन-कोश, प्राण-कोश एवं स्थूल शरीर-कोश से आच्छादित है, एक क्रमिक विधि को प्रस्तुत करता है। यह गहन चिन्तन द्वारा समीक्षित एवं वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषित विधि है।
राजयोग
अब हमें यह देखना है कि योग कितने प्रकार के होते हैं।
योग अनन्त हैं। कोई भी पदार्थ जिससे आपको दुःख से मुक्ति मिलती है और सच्चे आनन्द की प्राप्ति होती है, योग कहलाता है। योगाभ्यास विविध भाँति के हैं; परन्तु योग एक ही है। विविध अभ्यास-पद्धतियाँ लोगों की भिन्न-भिन्न क्षमता एवं रुचि के अनुरूप हैं। भिन्न-भिन्न लोगों के स्वभाव एवं योग्यता के अनुसार ही पूर्वजों ने विविध मार्गों को निर्धारित किया। यह पहली विचारणीय बात है कि ये मार्ग एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सब मार्ग अन्ततः एक ही समान प्रक्रिया का निर्देश करते हैं। आप तीन और सात का योग (जोड़) करें, चार और छह का करें, पाँच और पाँच का करें, आपको योग तो दस ही मिलेगा। इसी प्रकार योग-क्रम प्रत्यक्ष रूप में ही अलग-अलग दिखायी देता है; परन्तु उनकी अनुवर्ती मूल-प्रक्रिया एक ही समान है।
वह मूल-प्रक्रिया कौन-सी है?
बुद्धिमान् कहते हैं कि एक आवरण है जिससे तथ्य छिपा हुआ है तथा ईश्वर के सम्बन्ध में इसे माया कहते हैं और जीवात्मा के सम्बन्ध में इसे आवरण कहते हैं। जीवात्मा व्यक्तिगत चैतन्य में ढक (निहित हो) जाती है। इस आवरण के दूर होने पर उसे परमात्मा से एकरूपता का ज्ञान हो जाता है। योग का उद्देश्य इस आवरण को दूर करना है। ज्ञानयोग, भक्तियोग एवं राजयोग-सबका यही उद्देश्य है। वे मनुष्य के एक रूप को ले कर उसके द्वारा उसको इस योग्य बनाते हैं कि वह परमात्मा से अपनी समरूपता का ज्ञान कर सके।
मनुष्य बुद्धि, भाव एवं अन्तरावलोकन की गुह्य क्षमता से युक्त है। इन तीनों क्षमताओं में से जिस व्यक्ति में जो क्षमता प्रबल होती है, उसी के अनुरूप योगाभ्यास उसके अनुकूल होता है। यदि बुद्धि-प्रधान है तो साधक ज्ञानयोग का आश्रय लेता है, भावना-तत्त्व होने पर परम सत्य की प्राप्ति हेतु भक्तियोग को अपनाता है तथा अलौकिक तत्त्व अन्तरावलोकन की क्षमता का अतिरेक होने पर राजयोग अपनाया जाता है। राजयोग को ध्यानयोग भी कहते हैं। कर्मयोग से तो आप सब लोग परिचित ही हैं। आप ज्ञानयोगी हों, भक्तियोगी हों अथवा ध्यानयोगी हों, कर्मयोग तो परमावश्यक है। फल से अनासक्त रह कर इस संसार में कर्म करने के रहस्य को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग का रहस्य अनासक्ति है। अनासक्त कर्म ही बन्धनों से मुक्त कर सकता है।
राजयोग उनके लिए है जो स्वभाव से रहस्यवादी एवं अन्तर्मुखी हैं।
इसमें आगे कैसे बढ़ा जाये ?
राजयोग में आठ विभिन्न सोपान हैं; अतः इसे अष्टांगयोग भी कहते हैं। ज्ञानयोग की प्रथमावस्था में साधक के लिए कुछ आवश्यक गुण आचक्षित हैं-साधन-चतुष्टय अर्थात् विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति जैसे शम, दम, तितिक्षा आदि और अन्ततः मुमुक्षुत्व-मोक्ष के लिए अतीव प्रबल इच्छा और अभिलाषा। इन गुणों से युक्त होने के उपरान्त परम सत्य के स्वरूप का श्रवण करने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। इसके पश्चात् श्रवण किये हुए का चिन्तन करना चाहिए। इसे मनन कहते हैं। अब निरन्तर उस पर ध्यान करें। इसे निदिध्यासन कहते हैं। जिस प्रकार ये साधन-चतुष्टय ज्ञानयोग के अंग हैं उसी प्रकार राजयोग के आठ अंग हैं। महर्षि पतंजलि ने इस योग का निरूपण किया; अतएव इसे पातंजलयोग भी कहते हैं। राजयोग सब योगों से अधिक वैज्ञानिक एवं युक्तिसंगत है। साधारणतया योग शब्द राजयोग को ही निर्दिष्ट करता है। योग-दर्शन का अभिप्राय है पतंजलि का अष्टांगयोग। राजयोग इसका पारम्परिक नाम है। वस्तुतः सब मार्ग ध्यान-अवस्था में पर्यवसित होते हैं; क्योंकि राजयोग में ध्यान का बहुत महत्त्व है, अतएव इसे ध्यानयोग भी कहते हैं।
राजयोग के आठ अंग हैं : यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । इनमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम प्राथमिक अवस्थाएँ हैं। वास्तव में योग प्रत्याहार से आरम्भ होता है। प्रत्याहार का अभिप्राय है मन और इन्द्रियों को प्रमादशून्य कर अन्तर्मुखी करना। यम का अर्थ है कुछ विशेष गुणों का अनुशीलन करना अथवा अभिवृद्धि करना। नित्य व्रतों का पालन करना नियम है। शरीर को सर्वथा निष्क्रिय एवं स्थिर करके (एक विशेष ढंग से) बैठना आसन कहलाता है। आन्तरिक, सूक्ष्म स्नायविक प्रवाह से सम्बन्धित स्थूल प्राण (श्वास) का अनुशासन, संयम तथा नियमन प्राणायाम है। मन और इन्द्रियों को बाह्य विषयों से अन्तर्मुख करना प्रत्याहार कहा जाता है और ध्यान के विषय पर मन को एकाग्र करने का नाम धारणा है। धारणा पर प्रभुत्व प्राप्त करके ध्यान के विषय पर चित्तवृत्ति को निरन्तर स्थिर करना ध्यान है। धारणा में अस्थिरता होती है; परन्तु इस पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेने के पश्चात् चित्तवृत्ति को स्थिररूपेण बहुत समय तक ध्यान के विषय पर एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान की गहराइयों तक पहुँचने के उपरान्त आप निम्न स्थूल चेतना का अतिक्रमण करके चित्-शक्ति को प्राप्त करते हैं। यह समाधि-अवस्था कहलाती है।
यहाँ हठयोग तथा राजयोग के आसनों में अन्तर देखना है। राजयोग में हठयोग के चौरासी लाख आसनों का विवरण नहीं मिलता। ध्यानाभ्यास हेतु स्थिर रूप से बैठने का कोई भी ढंग राजयोग में आसन कहा जाता है। हठयोग में आसन का अभिप्राय कुछ और ही है। राजयोग में आसन की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है : 'स्थिरसुखमासनम्' (पा. यो. २-४६) -शरीर को किसी एक मुद्रा में स्थिरता से सुखपूर्वक टिकाये रख कर बैठना। कोई भी सुखदायक मुद्रा, जिसमें आप शरीर को अधिक देर तक स्थिर रख सकते हैं, आसन कहलाती है। प्राणायाम अथवा प्रत्याहार करने वाले किसी भी योगी के लिए आवश्यक है कि वह कम-से-कम तीन घण्टे तक एक आसन में बैठ सके। इस भाँति हमें राजयोग एवं हठयोग के आसनों के बीच भेद देखना है।
राजयोग सर्वप्रथम स्थूल शरीर को संयत करने में सहायक होता है। फिर शनैः-शनैः सूक्ष्म कोश यथा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनन्दमय कोश को संयत करने की विधि सिखाता है और हमें उस शाश्वत, नित्य-पूर्ण आत्म-तत्त्व की ओर ले जाता है जो इन सब कोशों से परे है। अतएव साधना का क्रम बाह्य शरीर से आरम्भ होता है और सूक्ष्म शरीरों की ओर बढ़ता है। अतः आभ्यन्तर शुद्धि तथा आत्म-सिद्धि के लिए राजयोग एक अतीव वैज्ञानिक एवं युक्ति-युक्त विधि है।
यम
पतंजलि ऋषि ने सर्वप्रथम सर्वथा बाह्यतः दृष्टिगोचर शरीर को ही लिया। आप जानते ही हैं कि मन के बाह्य, स्थूल एवं भौतिक स्वरूप का प्रकटीकरण शारीरिक क्रिया के रूप में होता है। इसीलिए उन्होंने विचार किया कि पहले मन के मल को दूर किया जाये एवं उसके प्रभाव तथा लक्षणों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाये। उनके अनुसार लक्षणों द्वारा ही कारण विद्यमान रहता है। ज्यों-ज्यों हम मानसिक वृत्तियों को कर्म-रूप में अभिव्यक्ति देते हैं, त्यों-त्यों वे और पुष्ट होती जाती हैं। अतः असली बात मन को वश में करना है। फिर भी, ध्यानावधि में प्राप्त, पतंजलि के अनुसार, विचार पर कर्म की भी प्रतिक्रिया होती है। हर बार आपकी क्रिया आपके कर्म को प्रबल बनाती है। युक्तियुक्त निष्कर्ष यह है कि बाह्य क्रिया तक पहुँचने पर विचार प्रवेग प्राप्त कर लेते हैं। आप कम-से-कम, इसके अत्यन्त स्थूल भौतिक रूप को तो नष्ट कीजिए, यद्यपि सदाचारवादी[3] तो इस बात का विरोध ही करेगा। उसके अनुसार क्रिया को निरुद्ध करने से कोई लाभ नहीं, मन को ही बदलना चाहिए।
परन्तु यह कार्य इतना सुगम नहीं। मन को सीधे ही वशीभूत करना अति-कठिन है। मन वही करता है जो उसकी इच्छा होती है। वह जो भी कल्पना करता है, वह क्रिया-रूप में परिणत हो जाती है। सर्वप्रथम इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाइए। जहाँ भी यह क्रिया-रूप में स्वयं को व्यक्त करना चाहे, आप कहें, 'नहीं'। इसकी बाह्य क्रियाओं के विरुद्ध युद्ध ठान लीजिए। मन के परिवर्तन को ही वास्तविक योग समझने वाले अविचारी मनुष्य को संकल्प (यम) एवं व्रत (नियम) मूर्खतापूर्ण दिखायी दे सकते हैं; परन्तु जो व्यक्ति इस अवस्था को पार कर चुका है, उसके लिए भी इनका कोई महत्त्व नहीं; किन्तु प्राथमिक अवस्थाओं में हम इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। हम जो अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं, हमें इनका उतना ही महत्त्व जानना चाहिए जितना कि आगे वाली अवस्थाओं का होगा। अनुमान करें, एक सीढ़ी है। उसमें सोपान ऐसे लगे हैं कि आप (ऊपर चढ़ने के लिए) एक सोपान भी छोड़ नहीं सकते; परन्तु यदि आप फिर भी यह कहें कि आपको प्रथम सोपान नहीं चाहिए तो आप सदा भूमि पर ही रहेंगे।
मन बहुत कपटी है। यह कोई-न-कोई बहाना ढूँढ़ ही लेता है। यह आदर्श उपस्थित करता है, 'मैंने अपने पूर्व-जीवन में उस अवस्था को पार कर लिया है। अब यदि मैं पाँच प्याले चाय पी लूँ और मांस भक्षण करूँ तो कुछ हानि नहीं होगी।' ऐसा कहने वाला व्यक्ति अपनी जिह्वा का दास होता है। वह मांस भक्षण नहीं छोड़ सकता। मांस भक्षण त्यागने का आशय होगा कि आप अपने मन पर प्रभुत्व जमा रहे हैं अर्थात् मन को संयम में रख रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि आप प्रातः चार बजे उठ कर ठण्ढे जल से स्नान करेंगे तो इसका आशय है असत् निम्न प्रकृति के प्रभाव पर आध्यात्मिक प्रकृति के उत्कर्ष को निरन्तर एवं पुनः-पुनः स्थापित करना। आप अपनी उच्च अलौकिक प्रकृति से निम्न लौकिक प्रकृति को अकस्मात् ही अलग नहीं कर सकते। उन्हें पृथक् करने के लिए आपको सात्त्विक संकल्पों का अनुष्ठान करना होगा। परन्तु यह भी स्मरण रखना होगा कि अपनी रुचि के कुछ विशेष पदार्थों का त्याग ही योग नहीं है, पर वास्तविक योग तक पहुँचने के लिए ये अभ्यास आवश्यक अवश्य हैं। तभी पतंजलि ऋषि ने कहा था, 'सर्वप्रथम आप अपनी बाह्य प्रकृति को संयत करें।' यदि आप इच्छाओं को एकदम से नियन्त्रित नहीं कर सकते तो कम-से-कम शारीरिक क्रियाओं पर तो संयम प्राप्त कर ही लें।
शारीरिक क्रिया का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यह तो सब जानते ही हैं। आप किसी भी अनुरक्ति का निरन्तर चिन्तन कर सकते हैं, पर उसे क्रिया-रूप में लाने पर मन को जो आघात पहुँचता है, वह बहुत बड़ा है। कल्पना द्वारा मनस्तत्त्व पर पड़ने वाला आघात उतना बड़ा नहीं होता जितना कि वास्तविक कार्य द्वारा पड़ने वाला होता है। कर्म मनुष्य की स्मृति का एक ठोस अंग बन जाता है और उसे विचारने या कल्पना करने से कहीं अधिक क्षुब्ध करता है। इसीलिए पतंजलि ने कहा है कि पहले सब कर्मों को शुद्ध करो और उन पर नियन्त्रण रखो। परन्तु कैसे ? उन्होंने बताया कि कुछ विशेष संकल्प लो और अपने आचार-व्यवहार को सार्वलौकिक नियमों के अनुकूल ढालो। वे नियम कौन-से हैं? वे यम के अन्तर्गत आते हैं। संकल्प कीजिए कि आप सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि का पालन करेंगे।
यम पाँच हैं। प्रश्न उठता है कि पाँच ही क्यों, ये दश अथवा अधिक क्यों नहीं? किन्तु यह भी ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित है। यदि आपमें पाँच मूल सार्वलौकिक गुण घर कर लें तो शेष सब सामान्य सद्गुण स्वतः ही आपमें आ जायेंगे। इन मूल गुणों को पतंजलि सार्वलौकिक संकल्प कहते हैं अर्थात् ऐसे संकल्प जिनका पालन प्रत्येक दशा, प्रत्येक स्थान एवं समय पर किया जाये। ये संकल्प हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह। यदि साधक निश्चय कर ले और इन संकल्पों के अनुष्ठान के लिए संघर्ष करे तो उसमें समस्त बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। समस्त अयुक्त कर्म झूठ, बेईमानी, कपट, लोभ, अपवित्रता, इन्द्रिय-लिप्सा, काम या क्रूर स्वभाव अथवा दूसरों को हानि पहुँचाने से होते हैं। इस प्रकार एक बुरे या दुष्ट व्यक्ति के सभी कर्म झूठ, क्रूरता, इन्द्रियासक्ति, लोभ अथवा अन्य की सम्पत्ति छीनने की प्रवृत्ति आदि कोई-न-कोई अवगुण तो व्यक्त करेंगे ही। यह निष्कर्ष पतंजलि ऋषि का है। उनका सभी साधकों से आग्रह है कि वे कुत्सित विचारों की बाह्य अभिव्यक्ति, कुटिल प्रयोजन एवं बुरे भावों को समाप्त करके, अपने कृत्यों को पाँच महान् एवं सार्वलौकिक संकल्पों-प्रेम, सत्य, ब्रह्मचर्य, अलोलुपता तथा अस्तेय-के अनुरूप बनायें। यह संकल्प ही मन की अधम प्रकृति के दिव्यान्तर का आधार और इसे बाह्य अभिव्यक्तियों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। ऋषि पतंजलि परिधि से केन्द्र की ओर अग्रसर होते हैं।
इतना तो हम जान ही चुके हैं कि शारीरिक अनुशासन की बहुत आवश्यकता है; क्योंकि मन पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मन में यदि कुत्सित विचार उत्पन्न हों तो उनके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न कृत्यों को निर्मूल करना हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार एक स्नायु के निष्क्रिय होने पर वह संकुचित हो कर क्षीण हो जाती है उसी प्रकार मन के भौतिक कर्म क्षीण हो जाते हैं और इस प्रकार एक आदत बन जाती है। विचार के आने पर मन इन्द्रियों को निरन्तर संयत करता हुआ कर्म में लग जाता है और यह आदत निरोध की तरह कार्य करती है। निरोध का अभिप्राय प्रतिबन्ध लगाने वाली किसी भी वस्तु से है। आप मन की हिंस्र प्रकृति को ही प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। बुरे कर्म का प्रत्युत्तर अच्छे कर्म से दो, यही यम है। मन की अधः प्रवृत्ति को वशीभूत करने की दिशा में किये गये प्रयत्न की यह प्रथमावस्था है।
अहिंसा
प्रथम यम है 'अहिंसा' अर्थात् किसी को दुःख न देना। इस सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। प्रथम तो यह कि अहिंसा का अर्थ केवल किसी ही हत्या न करना ही नहीं, अपितु कष्ट न देना भी है। अतएव, किसी भी जीव को किसी भाँति का कष्ट न देना अथवा हानि न पहुँचाना अहिंसा है। द्वितीय बात है सार्वलौकिक संकल्प (व्रत) यम के अन्तर्गत आते हैं। वे वर्ग, समय, स्थान, परिस्थिति आदि की सीमा से बाहर हैं। एक अभिकांक्षी साधक को दृढ़तापूर्वक प्रत्येक अवस्था या समय में इन पर अडिग बने रहना चाहिए। इनका अभ्यास अनियमित अथवा इच्छानुरूप चाहे कभी भी नहीं होना चाहिए। यह (व्रत) आपके जीवन को शासित करने बाले अति-महत्त्वपूर्ण नियम बन जाने चाहिए।
आध्यात्मिक जीवन में अहिंसा का विशेष महत्त्व क्यों है? यमों में इसका स्थान प्रथम क्यों है ? इसका वास्तविक आशय क्या है? यह सब समझने के लिए आप क्षण-भर विचार करें कि आध्यात्मिक जीवन और साधना का अर्थ एवं प्रयोजन क्या है।
अपूर्ण, सीमित मानुषिक सत्ता को उसके मूल, आध्यात्मिकता के असीम, अलौकिक एवं दिव्यालोक में परिणत करने का क्रम साधना कहलाता है। मनुष्य की एक अधम, पाशविक प्रकृति होती है, एक मानवीय प्रकृति और एक आन्तरिक तात्त्विक दिव्य प्रकृति होती है जो उसका वास्तविक आत्म-स्वरूप है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है पाशवी प्रकृति पर विजय एवं संयम प्राप्त करके मनुष्य का दिव्य स्वभाव में उदात्तीकरण।
अब, उपर्युक्त प्रकाश में हमें देखना है कि हिंसक पशु का मुख्य लक्षण क्या है। लक्षण है उग्रता एवं क्रूरता। अतएव अधम पाशविक प्रकृति पर मनुष्य की विजय का प्रथम चरण है अकुलीन विकट प्रवृत्तियों को ही नष्ट कर देना। और तो और अत्यन्त सुसभ्य, सुसंस्कृत, शिक्षित एवं शिष्ट लोगों में भी यह लक्षण विद्यमान रहता है; स्त्रियों में भी। उच्च कुल के कहे जाने वाले रईस (कुलीन) लोगों में भी विकृत सम्भोग में क्रूर व्यवहार करने की लालसा रेखा की तरह देखने को मिलती है। माता-पिता का बच्चों के प्रति, स्वामी लोगों का सेवकों के प्रति, सास का बहू के प्रति एवं निर्दयी पति का पत्नी के प्रति कठोर एवं बुरा व्यवहार आधुनिक समाज में सर्वत्र ही चलता है और इसकी अभिव्यक्ति का माध्यम एवं रूप है क्रोध। इसलिए महर्षि पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट अहिंसा अर्थात् मन, वचन तथा कर्म से किसी जीव को दुःख न पहुँचाने का व्रत साधक की पाशवी प्रवृत्ति को दूर करने का सर्वोत्तम एवं अत्यन्त प्रभावपूर्ण साधन है।
इसके अतिरिक्त, देवत्व-प्राप्ति का आशय है सात्त्विक प्रकृति का विकास एवं परिस्फुटन। दैवी सम्पद् अथवा दिव्य स्वभाव के अर्जन की आवश्यकता है। ईश्वर प्रेम-स्वरूप है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें किसी जीव को किसी प्रकार भी दुःख अथवा हानि न पहुँचायी जाये। हिंसा और अत्याचार प्रेम के सर्वथा विरुद्ध हैं। शान्तं, शिवं, शुभम् ही भागवतीय सत्ता का स्वरूप है और इसलिए अहिंसा को सद्गुणों में सर्वोच्च स्थान मिला है। कहा भी है- 'अहिंसा परमो धर्म:।' अतएव राजयोग के पाँच यमों में इसे प्रथम स्थान दिया गया है।
द्वार पर आये हुए भिखारी का कठोरता से निरादर करना अहिंसा-व्रत को भंग करने के समान है। किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए वचन दे कर या आशा बँधा कर, बिना सोच-विचार किये उसे निराश करना अहिंसा को भंग करना है। दूसरों के समक्ष, किसी व्यक्ति की अवज्ञा करना अथवा उसके प्रति जानबूझ कर अशिष्टता दिखाना निरंकुश क्रूरता है। कठोर एवं अविनीत वचन हिंसा है। किसी अन्य से हानिप्रद कार्य करवाना अथवा उसके क्रूर कर्म का अनुमोदन करना अहिंसा की प्रतिज्ञा भंग करना है। किसी के दुःख-निवारण में असफल होना अथवा दुःख के समय किसी व्यक्ति की सहायता हेतु जाने की उपेक्षा करना भी एक प्रकार की हिंसा है, यह प्रत्यवाय पाप है। यदि आप अहिंसा के साधक बनना चाहते हैं और सचमुच में ही अपनी साधना के प्रति गम्भीर हैं और वास्तव में ही शुद्धहृदयेन शाश्वत आनन्द और कैवल्य की प्राप्ति के लिए उन्नति करना चाहते हैं तो प्राणिमात्र को हाव-भाव से, आकृति से, कर्कश वाणी से अथवा अविनीत शब्दों से कष्ट देना सर्वथा त्याग दें। आप जो भी अभ्यास करते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से करिए। दैवी गुण अहिंसा के साकार रूप बन जाइए।
सत्य
महर्षि पतंजलि द्वारा साधकों के अभ्यास के लिए निर्धारित सार्वलौकिक नियमों में द्वितीय नियम है-सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करना। सत्य-स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको सर्वथा सत्यनिष्ठ बनना होगा। सत्य का साक्षात्कार करने के लिए सत्य में ही जीना होगा, सत्य-स्वरूप ही बनना होगा तथा सत्य के प्रति आंशिक नहीं, सम्पूर्ण और सर्वोपरि लगाव रखना होगा। साधक-जीवन की नींव रखने के लिए यह दूसरा तत्त्व है।
जैसा कि 'अहिंसा' के सन्दर्भ में पहले भी बताया जा चुका है, आपको स्मरण रखना है कि इन यम-नियमों को साधक अथवा सत्याकांक्षी को सामान्य व्यावहारिक ढंग से नहीं, अपितु एक विशेष आशय से पालन करना है। साधक के लिए इनका प्रयोजन नैतिक अथवा धार्मिक विषय से कहीं बढ़ कर है। आध्यात्मिक रूप से इसका विशेष महत्त्व है। आत्मा परम सत्य है। अन्य सब दृग्विषय मात्र हैं, असत्य हैं। इस प्रकार सत्य का पालन करने का आशय है संसार, जो असत्य है, से विमुख हो कर आध्यात्मिकता, परम सत्य के प्रति निष्ठा और भक्ति व्यक्त करना। स्मरण रहे, ईश्वर सत्य है और सत्य के द्वारा ही उसका साक्षात्कार सम्भव है। सत्य का आचरण करना जानते हुए इस प्रार्थना-'असतो मा सद्गमय' - 'मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल' में यथार्थ रूप से जीना है।
सत्य सार्वभौम नियम है। सब पदार्थ इस ईश्वरीय नियम का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक तत्त्व अपनी प्रकृति के प्रति सत्य है। इस ब्रह्माण्ड की प्रत्येक शक्ति अपने स्वरूप के प्रति सत्य है। प्रत्येक ग्रह निर्धारित मार्ग के अनुसार परिभ्रमण करता है। इसके बिना सृष्टि-क्रम अस्त-व्यस्त हो जाये। अनुमान कीजिए, यदि अग्नि उष्णता अथवा दाहकता त्याग दे, जल अपनी तरलता और शीतलता छोड़ दे और वायु चलना बन्द कर दे तो सृष्टि की क्या दशा होगी। अतः सत्य ही इन सबका सम्पोषक तत्त्व है। आध्यात्मिक साधना एवं दिव्य जीवन के आधार-रूप धर्म का सार और मूल सत्य ही है। तभी तो सत्य को सहस्र अश्वमेध यज्ञों से भी श्रेष्ठ माना गया है। वेदों के अध्ययन और वैदिक ज्ञान से भी सत्य कहीं बढ़ कर है। अत: योगी और साधक के लिए पूर्णतया सत्यनिष्ठ बनना अतीव महत्त्वपूर्ण है।
आपको यम के इस नियम की सर्वोच्च महत्ता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सत्य से कभी विचलित न हों। अर्ध सत्य से कभी मेल न करें। मिथ्यात्व के बहुत से रूप और तथाकथित हानि-रहित असत्य आधुनिक समाज के घनिष्ट अंग बन गये हैं। अधिक प्रचलन अथवा परिपाटी झूठ को सदाचार नहीं बना सकते। नित्यानन्द एवं अमरत्व को प्राप्त करने के इच्छुक सच्चे साधक का किसी भी प्रकार के झूठ से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। चाटुकारिता भी सत्य न बोलने के समान है, आप दूसरे का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए लज्जा त्याग कर जो-कुछ बोल देते हैं, वह वास्तविकता नहीं होती। अतिशयोक्ति झूठ का एक अन्य रूप है। आप इसका प्रयोग जन-मानस में सनसनी उत्पन्न करने और महत्त्व प्राप्त करने के लिए करते हैं। छल-कपट और कूटनीति भी घृणित पाप है। सत्यशील और सरल बनें। निष्कपट बनें। यदि सत्य अप्रिय या दूसरे को कष्ट या आघात पहुँचाने वाला हो तो भद्रतापूर्वक विषय बदल दें या प्रेमपूर्वक मौन धारण कर लें। अहिंसा भी सत्य का एक अंश बन जानी चाहिए। बेईमानी के कार्यों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। कपटपूर्ण व्यवहार करना, उत्कोच (घूस) लेना और जन-प्रवाद फैलाना, यह सब सत्य के साथ भयंकर विश्वासघात करना है। इन सब पर विजय प्राप्त करने अथवा इनको नष्ट करने का उपाय है अपने अन्तःकरण की खोज। प्रतिदिन आत्म-निरीक्षण एवं आत्म-विश्लेषण करें। अपने स्वभाव और व्यवहार में असत्यता को ढूँढ़ें तथा उसके उन्मूलन का प्रयत्न करें। इस महत्त्वपूर्ण साधना में शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, दृढ़ निश्चय करें। आपको सफलता प्राप्त होगी। आप शीघ्र ही सत्य में प्रतिष्ठित हो जायेंगे।
सत्य धधकती हुई प्रचण्ड अग्नि के समान है। केवल सत्य के द्वारा ही निम्न प्रकृति के सब दाग (पाप) पूर्णतया मिट सकते हैं। जिस प्रकार बलवान् के पास शक्ति होती है उसी प्रकार साधक की शक्ति सत्य है। संसार के प्रलोभनों से बचने के लिए यह महा-कवच-रूप है। केवल सत्य के द्वारा ही सम्पूर्ण संसार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पूर्णरूपेण सत्य में अधिष्ठित व्यक्ति की वाणी से निकला वचन सर्वदा सत्य ही होता है। वही होगा जो वह सोचेगा। शनैः शनैः सत्य आपके जीवन को देवत्व में परिणत कर देता है। यह अमरत्व और असीम आनन्द की वर्षा करता है।
सत्य में निवास करो। सत्य के मूर्त-रूप बन जाओ। मन, वाणी तथा कर्म से सच्चे रहो। सत्य-स्वरूप होने का अभिप्राय है किसी भी पदार्थ को उसके वास्तविक रूप में कहना या व्यक्त करना। अतः सत्य का वास्तविक उपलक्षण अथवा अर्थ है जो आप वास्तव में हैं, वही दिखायी देना। यह भाव आपकी सच्चिदानन्द-स्वरूप दैविक प्रकृति अथवा शान्तं, शिवं, शुभं, सुन्दरम् नामक वास्तविक और शाश्वत प्रकृति को स्फुटित करता है। केवल झूठ से अलग रहना ही सत्य नहीं; अपितु मन, वचन तथा कर्म द्वारा अपने उपयुक्त सत्य स्वभाव को स्पष्ट करना भी सत्य है। अपने ही स्वभाव अथवा स्वरूप को ही झुठलाना सत्य के साथ विश्वास भंग करना है।
हे साधक! आप पवित्र दिव्य आत्म-स्वरूप हैं। पवित्र होना, आध्यात्मिक होना सत्यशील होते के समान है। देवत्वहीन होना, अशुद्ध होना अथवा असात्त्विक होना ही असत्य के समान है। आपकी पूर्ण सत्ता, आचरण एवं जीवन के प्रत्येक रूप में आपके आत्मिक स्वभाव के दर्शन होने (मिलने) चाहिए। जैसा कि भगवद्गीता में वर्णित है, सत्य सब दैवी सम्पदाओं का अभ्यास दर्शित करता है।
साधको! यदि आप सचमुच में ही साधनाभिकांक्षी हैं, आध्यात्मिकता में शीघ्र सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन-लक्ष्य तक पहुंचने के इच्छुक हैं तो किसी भी मूल्य पर सत्यनिष्ठ बन जाइए।
ब्रह्मचर्य
अब हम राजयौगिक यम के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय, 'ब्रह्मचर्य' पर विचार करेंगे। अध्यात्म-मार्ग के अनेक नियमों में इसका स्थान अद्वितीय है; क्योंकि इस मार्ग की विभिन्न उच्चतर भूमिकाओं की ओर उत्तरोत्तर बढ़ने के लिए यह साधक को बल और प्रेरक शक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य से आध्यात्मिक विकास सम्भव होता है। योगी के लिए ब्रह्मचर्य उसी प्रकार आवश्यक है जैसे विद्युत् से चलने वाली गाड़ी के लिए विद्युत्। इसके बिना साधक योग-मार्ग में उन्नति नहीं कर सकता।
किसी भी प्रकार की क्रिया अथवा आन्दोलन को कार्यशील अथवा प्रेरित करने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म एवं उत्तम क्रिया को कार्यशील करने के लिए उसके अनुरूप ही अर्थात् सूक्ष्म एवं उत्तम शक्ति की आवश्यकता होगी। मानव-जीवन का सर्वोच्च एवं महानतम संघर्ष है उसकी आध्यात्मिक साधना। इसके लिए उच्च श्रेणी की प्रबल शक्ति एवं विशिष्ट प्रकार की स्नायविक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह शक्ति ब्रह्मचर्य के निष्ठायुक्त अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। केवल ब्रह्मचर्य की शक्ति द्वारा ही चंचल इन्द्रियों एवं कुटिल मन पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की जा सकती है। अतएव सब योगों में, सब साधकों को, चाहे वे कहीं भी हों और उनका कोई भी धर्म हो, इसी गुण पर आग्रह किया गया है।
ब्रह्मचर्य से यह परम शक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है?
इसके लिए चार क्रम हैं। मनुष्य के अन्दर एक रहस्यपूर्ण शक्ति का भण्डार है। यह शक्ति ही उसकी समग्र सत्ता को अनुप्राणित करती है। मानव में निहित यह शक्ति दो रूपों में प्रकट होती है। इन्द्रिय-शक्ति स्थूल रूप है जो चपल इन्द्रियों के माध्यम से निरन्तर विषयासक्ति-रूप में प्रकट होती रहती है। शक्ति का सूक्ष्म रूप आध्यात्मिक है जो आपको चेतना के ऊर्ध्व स्तर की ओर ले जाता है। निम्नतम स्तर पर यह दैविक वासना-शक्ति है और उच्चतम स्तर पर है ओज-शक्ति जो ज्ञानोत्कर्ष साधक अथवा योगी के गम्भीर ध्यान की गहन ज्वाला को देदीप्यमान करती है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है शारीरिक प्राण-शक्ति को शुद्ध और उदात्त करके आध्यात्मिक ओज-शक्ति में रूपान्तरित कर देना। इस प्रकार एक प्रबुद्ध साधक के लिए ब्रह्मचर्य केवल निग्रह अथवा निरोध ही नहीं, अपितु एक स्पष्ट सजीव शक्ति-सम्पन्न परिवर्तन-क्रम है। अतः यह प्रक्रिया चतुर्विध है-पाशवी शक्ति को संयमित करना, संरक्षण करना, उच्च स्तर की ओर उन्मुख करना और अन्ततः ओज-शक्ति में परिवर्तित कर देना।
तृष्णा के अधीन इन्द्रियों द्वारा आपकी शक्ति स्रवित होती रहती है। शक्ति का यह अपव्यय समाप्त होना चाहिए। आत्म-संयम, दम अथवा इन्द्रियनिग्रह ब्रह्मचर्य के लिए अपरिहार्य हैं। इस प्रकार साधक के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम-प्रवृत्ति पर नियन्त्रण करना ही नहीं, अपितु प्रत्येक इन्द्रिय को संयम में करना है जिससे काम पर विजय प्राप्त की जा सके। यह सर्वव्याप्त दम है। आपके सम्पूर्ण जीवन एवं कृत्यों में ब्रह्मचर्य-भावना परिव्याप्त होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य द्वारा प्राप्त बल को सावधानी से सुरक्षित रखना चाहिए। अमूल्य सम्पत्ति की भाँति इसका संरक्षण करना चाहिए। एक सच्चा साधक प्राण त्याग सकता है, परन्तु ब्रह्मचर्य नहीं खोयेगा। जीवन के प्रत्येक क्षण में अविरत जागरूकता एवं सात्त्विक विचार से आप इसकी रक्षा कर सकते हैं। स्वयं को इस मूढ़ कल्पना से बचाना चाहिए कि कुछ वर्ष अकेले रह कर, थोड़ी सात्त्विकता और पवित्रता का अनुभव करके आप सोचने लगें कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली।
मनुष्य में काम-प्रवृत्ति गहरी जड़ जमाये है। मनुष्य की अस्तित्व-रचना में यह सबसे पुरातन प्रवृत्ति है। सृष्टि के आरम्भ से ले कर युगपर्यन्त के विकास के मध्य पुनर्जन्म एवं बहुत्व की उत्कट कामना काम-शक्ति द्वारा सजीव चली आ रही है। अतः शक्ति को संयमित करने तथा संरक्षण में रखने के प्रयत्न करने पर भी यह बलपूर्वक अपने को प्रकट करने का प्रयास करती है और साधक को आकुल कर देती है। यहीं आवश्यकता उठती है बुद्धिमत्तापूर्वक इस शक्ति को उपयुक्त उपाय द्वारा पवित्र दिशा की ओर मोड़ने की। आसन, प्राणायाम, मुद्राएँ, क्रिया, कर्मपरक सेवा एवं सब प्रकार की विशुद्ध कर्मशीलता इसे अन्तर की ओर मोड़ कर ऊर्ध्व-गतिशीलता देने में सहायक होती है। ब्रह्मचर्य का एक महत्त्वपूर्ण रहस्य है मन को साधना में निरन्तर लीन रखना।
धीरे-धीरे यह शक्ति शुद्ध अध्यात्म-शक्ति में बदल जाती है। यह साधना द्वारा ही परिवर्तित की जाती है। इस परिवर्तन या उदात्तीकरण का परिणाम है ओज-शक्ति, जिसके द्वारा साधक धारणा तथा ध्यान करने के योग्य बन कर गहन समाधि में प्रवेश कर सकता है।
अब आप ब्रह्मचर्य की महत्ता समझ गये होंगे। जो साधक इस महत्त्वपूर्ण यम की अवज्ञा करता है, वह आध्यात्मिक जीवन में कभी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता। मन, वचन तथा कर्म में पूर्ण शुद्धता के प्रतिरूप ब्रह्मचर्य के बिना साधना असम्भव है। साधक का प्रत्येक विचार और उसकी भावना स्फटिक के समान शुभ्र (पवित्र) होनी चाहिए। उसका चरित्र दोष-रहित होना चाहिए। थोड़ी भी विषयासक्ति अथवा काम-भावना ब्रह्मचारी की प्रकृति को दूषित न करे। पवित्रता के लिए आपको प्रत्यक्ष राग से प्रेरणा मिलनी चाहिए। सर्वथा पवित्र बनने की ज्वलन्त कामना आपमें होनी चाहिए। ऐसी अवस्था हो कि काम-भावना ही कभी मन में उत्पन्न न हो। यही मानदण्ड है जिस तक पहुँचने के लिए प्रत्येक साधक को इच्छुक होना चाहिए।
ब्रह्मचर्य के प्रति रूढ़िवादी विचार भ्रामक हैं। साधारण भाषा में कौमार्यावस्था को ही ब्रह्मचर्य माना जाता है। बहुधा प्रश्न किया जाता है-"आप विवाहित हैं अथवा ब्रह्मचारी ?" आजकल यह हमारी संस्कृति की अधोगति है। ब्रह्मचर्य का गौरव एवं उसकी महत्ता भुला दी गयी है। एक सच्चा ब्रह्मचारी पृथ्वी पर साक्षात् भगवान्-स्वरूप है। इसलिए श्री शुक, भीष्म, हनुमान्, लक्ष्मण आदि महान् पुरुषों का आज भी स्मरण कर उनकी पूजा की जाती है। केवल कौमार्यावस्था ही ब्रह्मचर्य नहीं है। आध्यात्मिक साधना के लिए इसका आशय बहुत गहरा है। यह सत्य का अनुसरण करता है। पूर्ण शुद्धता देवत्व का आवश्यक गुण है। आपका सत्य-स्वरूप दिव्य है। यदि हम अपने स्वभाव और अन्तर्वासी आत्मा के प्रति सच्चे हैं और सत्य को ही अभिव्यक्त करते हैं तो अपने श्वास, विचार, वाणी एवं कर्म के प्रत्येक क्षण में हमें ज्ञान एवं इच्छापूर्वक अपने इस महान् आन्तरिक स्वभावपूर्ण पवित्रता को स्फुटित करने का यत्न करना चाहिए। केवल इस प्रकार ही आप वास्तव में ब्रह्मचर्यनिष्ठ बन सकेंगे। ऐसा ब्रह्मचर्य ब्रह्म-साक्षात्कार की ओर ले जायेगा।
अस्तेय
पूर्व परिच्छेद में आपको राजयौगिक यम के तीन महत्त्वपूर्ण गुणों के विषय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसी के अन्तर्गत चतुर्थ गुण है अस्तेय अथवा चोरी न करना। आश्चर्यजनक-सा प्रतीत होता है कि ऐसा नियम भी क्यों बनाया गया? हम इसे साधारण कमजोरी समझ सकते हैं; परन्तु अवश्य ही कोई महत्त्वपूर्ण कारण होगा जिससे महर्षि पतंजलि ने इस पर अंकुश रखने का विधान बनाया। यह अवगुण सर्वत्र दर्शनीय है। यह दुर्गुण किस प्रकार सर्वत्र व्यापक है, यह अभी स्पष्ट हो जायेगा जब हम मानव-चरित्र में इस लक्षण के विविध रूपों पर विचार करेंगे।
आपके लिए वस्तुतः जितना आवश्यक है, उससे अधिक पर अधिकार करने के लिए जो भी कार्य किया गया हो, वह विशुद्ध नैतिक एवं आध्यात्मिक मानदण्ड की दृष्टि से एक प्रकार की चोरी कहा जायेगा। आवश्यकता से अधिक खाना भी स्तेय (चोरी) माना जाता है। विलासिता पर किया गया व्यय भी चोरी है; क्योंकि इससे आप दूसरे को ऐसे पदार्थ से वंचित करते हैं जो उसके लिए उपयोगी हो। धन इकट्ठा करना चोरी है। किसी प्रकार का अति-व्यय, विलासिता जो केवल दिखावटी अथवा झूठी शान (सम्मान) के लिए व्यय है, चोरी कहा जाता है। सादा सरल जीवन व्यतीत करना ही अस्तेय के अनुष्ठान का सर्वोत्तम उपाय है।
आधुनिक सभ्यता ने सुख के लिए धन-व्यय के अनेक द्वार खोल दिये हैं। बचपन से ही बच्चे खरीददारी एवं मनोरंजन के लिए जेब-खर्च माँगते हैं। सिगरेट पीने, सिनेमा देखने, साइकिल की सवारी करने, क्रिकेट के मैच आदि देखने के लिए पिता अथवा बड़े भाई की जेब से चोरी करना साधारण बात है। दूसरे को बिना कहे कुछ चुरा कर ले जाना पाठशाला के बच्चे साधारणतया प्रशंसनीय चतुराई समझते हैं। इसे 'अच्छे मजाक' के रूप में लिया जाता है। इसके उपरान्त कालेज में जाने पर रेलवे स्टेशन पर टिकट-चेकर की बगल से धड़धड़ाते ऐसा स्पष्टोच्चारण करते हुए निकल जाना कि उनके पास 'पास' या 'सीजनल टिकट' है, सामान्य बात है, जब कि वास्तव में उनके पास इन दोनों में से एक भी अभिज्ञान-पत्र नहीं होता। कालेज के लड़कों के किसी दल के लिए रेस्टोरेन्ट में जा कर भोजन करना और पैसों का बिल बनाते समय गड़बड़ कर सेवक को बेवकूफ बनाना एक बहुत बड़ा मजाक समझा जाता है; परन्तु वास्तव में यह भी चोरी का ही एक रूप है।
सामान्य व्यक्ति को आधुनिक समाज में खोटा सिक्का चलाने अथवा दुकानदार द्वारा अज्ञान में अधिक दिये गये धन को चुपचाप जेब में रखने से कोई आत्मग्लानि नहीं होती। उत्कोच (घूस) द्वारा चीनी अथवा पेट्रोल प्राप्त करने के लिए अनुज्ञा-पत्र (परमिट) लेने में संकोच नहीं होता। राशन की वस्तुएँ 'ब्लैक' में ली जाती हैं और राशन बेचने वाला अनेक अनुज्ञा-पत्र वालों को कोई झूठा बहाना करके वापस कर देता है। धनी मुसाफिर 'विशेष प्रबन्ध' द्वारा अपने पालतू कुत्तों को गाड़ी का उचित टिकट खरीदे बिना यात्रा करवाने में सफल हो जाते हैं और अधिक सामान भी तथाकथित विशेष प्रबन्ध द्वारा बिना पैसों के ले जाते हैं। आधुनिक व्यक्ति का निर्माण इस प्रकार हुआ है। यह सब कृत्य 'स्तेय' (चोरी) के अन्तर्गत आते हैं। प्रत्येक गुप्त कार्य एवं जो कार्य आप दूसरों की दृष्टि से बच कर करना चाहते हैं, स्तेय के दृष्टिकोण से अपराध माना जाता है। जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान् प्रभु की सर्वव्यापकता में विश्वास रखता है, वह कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसमें चोरी या स्वायत्तता की गन्ध आती हो।
सामान्य व्यक्ति के अधिकांश कार्य स्वार्थ अथवा लालच के परिणाम-स्वरूप होते हैं। इन्द्रियाँ अनेक पदार्थों के लिए लालायित रहती हैं। आपकी कितनी ही कामनाएँ हैं। आपमें स्वयं के लिए भी अनेक वस्तुएँ प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। जब आप उन सबको प्राप्त नहीं कर सकते और अपनी कई इच्छाएँ सन्तुष्ट नहीं कर पाते तो आप उन्हें छल-कपट अथवा गलत उपायों द्वारा प्राप्त करने का यत्न करते हैं। यह सब प्राप्ति स्तेय (चोरी) के समान है। पूर्णतः ईमानदारी एवं सच्चाई द्वारा प्राप्त हुए पदार्थों से ही सबको सन्तुष्ट रहना चाहिए। किसी को भी ऐसी कोई वस्तु प्राप्त करने की कामना नहीं करनी चाहिए जो न्यायोचित रूप में उसकी न हो। ऐसी इच्छा ही अस्तेय का बीज-स्वरूप है। अस्तेय के प्रति आस्था भंग कर देना भोग-विलास की कामना को संयत न करने की अयोग्यता का परिणाम है। इन्द्रियों के शक्तिशाली होने पर अनियन्त्रित मन कई पदार्थों की कामना करता है, तभी छोटी-छोटी सामान्य-सी चोरियाँ करने की भावना मन में प्रवेश करती हैं। अतः चोरी का वास्तविक कारण अनगिनत कामनाएँ एवं अनियन्त्रित इन्द्रियाँ हैं। कामना एवं विषयासक्ति नैतिक भावना को अन्धा कर देती हैं और बुद्धि को निस्तेज बना देती हैं। किसी भी प्रकार की चोरी की भावना से दूर रहने के लिए आपको इच्छाओं को रोकना होगा, इन्द्रियों को अनुशासित करना होगा तथा मन को वश में करना होगा।
अपरिग्रह
यम का पाँचवाँ अंग है अपरिग्रह। इसका अर्थ है विलासिता के पदार्थों को स्वीकार न करना। उतना ही स्वीकार करो जितना सादा जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है, विषयासक्ति के लिए नहीं। निश्चित रूपेण, प्रत्येक व्यक्ति के रहने का स्तर भिन्न होता है। उदाहरणतया, एक राजा द्वारा की गयी अपरिग्रह की व्याख्या कृषक द्वारा की गयी व्याख्या से भिन्न होगी। एक कृषक को सादा भोजन, शायद चार रोटी और दाल लेने की आदत पड़ चुकी है; परन्तु यदि राजा भी कहे-'मैं चार रोटी और दाल खाऊँगा' तो उसे संग्रहणी (पेचिश) हो जायेगी। अतः आपको यह निश्चय करने में बुद्धि का प्रयोग करना है कि कौन-सा पदार्थ आपके जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक है और कौन-सा विलासिता के अन्तर्गत आता है। उष्ण प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति को कोट की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी; परन्तु शीत-मण्डल में रहने वाले व्यक्ति के लिए अपरिग्रह का अर्थ होगा न्यूनातिन्यून आवश्यकता से अधिक संख्या में कोट न रखना; क्योंकि यदि वह कोट को ऐश्वर्य-पदार्थ समझ कर पहनना छोड़ दे तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। तो आपको विदित होना चाहिए कि भगवान् ने आपको किस अवस्था में रखा है और इस भाँति आपको अपरिग्रह का अभिप्राय भी मालूम होना चाहिए।
जीवन में केवल अपरिहार्य आवश्यकताएँ ही रखनी चाहिए। एक स्थान पर गान्धी जी ने कहा कि जो मनुष्य आवश्यकता से अधिक खाता है, बह चोर है; क्योंकि इससे वह दूसरे को उस वस्तु से वंचित कर देता है जो उसकी आवश्यकता है। कभी भी आवश्यकता से अधिक द्रव्य संचित नहीं करना चाहिए और संचय करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। दूसरों से प्राप्त उपहार भी प्राप्तकर्ता पर प्रभाव डालता है। लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, अतः कई उद्देश्यों से उपहार लाते हैं। उपहार स्वीकार करने से स्वीकारकर्ता का मन अपवित्र हो जाता है। अतएव योग के अध्येता को उपहारों का परित्याग करना चाहिए। अपरिग्रह रक्षण की चिन्ता, क्षति का भय, क्षति का दुःख, घृणा, क्रोध, चोरी, मोह, निराशा, मन की व्याकुलता, अशान्ति, चिन्ता और क्लेश दूर करता है। इससे शान्ति, तृप्ति एवं सन्तोष प्राप्त होते हैं।
नियम
इससे पूर्व के पृष्ठों में हम देख चुके हैं कि महर्षि पतंजलिकृत अष्टांग योग की प्रथमावस्था 'यम' में पवित्रता की कितनी महत्ता है। योगाभ्यास से मनुष्य के स्वभाव की शुद्धि होती है और वह सदाचार में संस्थित हो जाता है। व्यावहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदाचार ही पर्याप्त है; परन्तु आध्यात्मिक जीवन में साधक कुछ विशिष्ट प्रकार का होता है जिसके समक्ष एक असाधारण लक्ष्य होता है जो उस साधारण सांसारिक व्यक्ति के आदर्श से सर्वथा उच्च एवं भिन्न होता है जिसे केवल बाह्य संसार का ज्ञान है, जिसके लिए सांसारिक पदार्थ ही बहुमूल्य हैं और जो संसार में विद्यमान पदार्थों को प्राप्त करने में ही दत्तचित्त रहता है। सांसारिक मनुष्य बाह्य दृष्टि रखता है, जब कि साधक अपनी विवेक-शक्ति तथा बुद्धि द्वारा यह जान लेता है कि विस्तृत दृश्य जगत् अल्पकालिक एवं क्षणिक है। ऐसे साधक जीवन के रंगमंच पर अल्पकाल के लिए आते हैं और अन्तर्धान हो जाते हैं।
कोई भी अस्थायी पदार्थ शाश्वत सन्तोष प्रदान नहीं कर सकता। नश्वर पदार्थ से जो सुख आप प्राप्त करते हैं, वह उस पदार्थ के नष्ट होने पर नहीं रहेगा। जब तक वह पदार्थ विद्यमान है, आप प्रसन्न हैं और जब वह पदार्थ नष्ट हो जाता है तो आपकी प्रसन्नता भी समाप्त हो जाती है। सुख का केन्द्र न रहने पर दुःख का अनुभव होता है। संसार के नश्वर पदार्थ आपको चिर-सन्तोष नहीं दे सकते। साधक तो शाश्वत सन्तोष प्राप्त करने में निरत रहता है-मिथ्या सन्तोष के लिए नहीं जो अन्ततः निराशा की ओर ले जाता है। साधक तो पूर्णता की वृष्टि करने वाले सन्तोष को प्राप्त करने में प्रयत्नशील होता है। उसकी मंजिल तो अन्ततः असीम के सर्वोच्च चैतन्य की प्राप्ति है जहाँ पहुँच कर कोई इच्छा नहीं, कोई ममता नहीं और इसलिए कोई दुःख भी नहीं। स्वयं को इस भाँति प्रतिबद्ध करके वह सोचता है कि केवल सदाचारिता ही पर्याप्त नहीं है।
जिसके लिए यह संसार ही सर्वस्व है, उसके लिए तो यही ठीक है; परन्तु साधक को तो द्वैत भाव से ऊपर उठना है और उस आत्म-तत्त्व की प्राप्ति हेतु, पूर्णावस्था का अनुभव करना है। वहाँ पहुँचने को ही वह प्रयत्नशील है। अतएव उसे आगे बढ़ना है, केवल धर्मपरायण अथवा पुण्यात्मा बन कर ही सन्तोष नहीं कर लेना है। चाहे सभी लोग उसकी पूजा भी क्यों न करें, स्वयं उसके अनुयायी भी क्यों न बन जायें, उसे तो उत्तरोत्तर बढ़ना है। अतः साधु एवं सदाचारी बनने के अतिरिक्त वह आध्यात्मिक बनने की भी अभिलाषा रखता है। उसे सदाचार से आध्यात्मिकता की ओर उठना है। यही उसका लक्ष्य है और इसीलिए दूसरे अंग 'नियम' का विधान किया गया है जो आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाले कुछ व्रतों से युक्त है।
हम देख चुके हैं कि महर्षि पतंजलि के विज्ञान का आधार मानव-रचना के अति-वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। उन्होंने संस्कृति, धर्म, सम्प्रदाय अथवा जाति से सर्वथा असम्पृक्त पार्थिव मानव का, मनुष्य को जिस रूप में प्रभु ने बनाया है और भूलोक में भेजा है, उसके उसी रूप में अध्ययन किया। अपने इस अध्ययन से उन्हें ज्ञात हुआ कि मनुष्य चैतन्य, ज्ञान एवं अस्तित्व का केन्द्र है और उसकी सत्ता का यह मुख्य तथ्य तीन सर्वथा भिन्न कोशों से ढका हुआ है। प्रथम है अन्नमय कोश, जो स्थूलतम तथा नश्वर है। द्वितीय है मनोमय कोश, जो चिन्तन-शक्ति से युक्त है, जिसमें विचार एवं भाव उत्पन्न होते हैं। मानव-जीवन की अर्हता मानसिक क्रियाओं पर ही निर्भर है। मन एवं शरीर को सूत्रबद्ध करने वाली व्यापक अद्भुत शक्ति चेतना, जो मन की क्रियाओं को कार्य रूप में परिणत करती है, मध्य का कोश है जिसे प्राणमय कोश कहते हैं।
अतः अन्नमय कोश, मनोमय कोश एवं प्राणमय कोश- इन तीन आवरणों के अन्दर जो मानव का विशुद्ध आत्म-तत्त्व है, वह सोचता है- 'मैं हूँ और यह सत्ता-तत्त्व अहं-चेतना (जीव-चेतना) द्वारा व्यक्त एवं प्रतिपादित किया जाता है जो चेतना का केन्द्र है। अपने व्यक्तित्व का अनुभव करते हुए जब वह अपने अस्तित्व को पहचानता है और उसकी सत्ता को मानता है (उसमें अहं-भाव आ जाता है), तब वह आत्म-चैतन्य के मूल तक पहुँचने की समस्या का सामना करता है और तब इस शरीर के प्रति असत् विचार उसके मन में आते हैं- 'मैं यह शरीर हूँ', 'मैं यह व्यक्ति हूँ', 'यह संसार है' -यह मिथ्या विचार मन में आते हैं। मन को रूपान्तरित करने के हेतु मनुष्य वैज्ञानिक रीति से स्थूलतम से सूक्ष्मतर शरीर की ओर, अपने शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने तक अग्रसर होता रहता है। सब विचारों के निःशेष हो जाने पर गहन ध्यान द्वारा उस स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। मन ही परमात्म-तत्त्व स्वरूप बन जाता है। सच्चिदानन्द पर ध्यान करने से मन सर्वरूपेण इन्हीं विचारों में निरत हो जाता है-'मेरी सत्ता है', 'मैं प्रकाश हूँ', 'मैं आनन्द हूँ', 'मैं ज्ञान हूँ।' मनुष्य में सहजावबोध जागृत करने के लिए ऐसा कहा गया है। यही ज्ञान उसे अपनी वास्तविक प्रकृति की पहचान एवं सत्य का साक्षात्कार करने योग्य बनाता है। यही चरमावस्था है।
प्रयत्न शरीर से ही प्रारम्भ होता है और इस वैज्ञानिक अभिनिवेश में महर्षि पतंजलि ने पहले शरीर के सर्वथा बाह्य पक्ष-स्वरूप कर्म को ही लिया है। कृत्यों को संयत करके उन्हें परिवर्तित कर सात्त्विक बनाना चाहिए। बुरे, कठोर एवं ध्वंसात्मक कर्म नहीं करने चाहिए। अतएव, कर्म को बदलने के लिए व्यक्ति के स्वभाव से कुवृत्तियों को दूर करने और उनके स्थान पर दिव्य गुणों को स्थापित करने हेतु एक व्यवस्थित प्रशिक्षण महर्षि पतंजलिकृत योग के लक्ष्य के प्रथम अति-वैज्ञानिक प्रयास को, जिससे साधक अपना कुटिल स्वभाव त्याग दे, यम कहते हैं। इसके अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं परिग्रह पाँच गुण सम्मिलित हैं।
अब हम नियम पर आते हैं जिसके अन्तर्गत दैनिक जीवन के कुछ अपरिहार्य व्रत समाविष्ट हैं। ये हैं-शौच (अन्दर और बाहर की शुद्धि), सन्तोष (तुष्टि), तपस् (तपस्या), स्वाध्याय (शास्त्राध्ययन) एवं ईश्वर-प्रणिधान (प्रभु के समक्ष आत्म-समर्पण)। इस नियम का उद्देश्य है-जीवनधारा को प्रभु की ओर प्रवाहित करना।
शौच
नियमों में प्रथम है शौच, शुचिता का अभ्यास, बाह्य एवं आन्तरिक शुद्धि। प्रारम्भ में शरीर की दशा का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः आपको शरीर भी निर्मलावस्था में रखना है जिससे कि शरीर के इस गुण का प्रतिबिम्ब मन पर भी पड़े। शरीर की अन्तः शुद्धि भी होनी चाहिए। आपको शुद्ध भोजन लेना चाहिए। यदि आप सूअर का गन्दा मांस खायेंगे तो आपका मन दूषित (गन्दा) हो जायेगा।
हमारे पूर्वजों ने पदार्थ को सत्त्व, रजस् एवं तमस्-इन तीन गुणों में विभक्त किया है। एक साधक का भोजन सात्त्विक होना चाहिए। क्यों? यह भी अनुभव तथा विशेष नियमों के अन्वेषण पर आधारित है। सब जानते हैं कि भोजन का शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भोजन का गुण तत्काल ही शरीर पर अपना प्रभाव दिखाता है। यदि आप अति-गर्म पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपको विसूचिका हो सकती है अथवा आपकी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वायु उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करने से बात-व्याधि हो सकती है। अत्यधिक बुरा भोजन अपना प्रभाव तत्काल दिखाता है। मदिरा पीने से मन तत्काल ही संयम से बाहर हो जायेगा। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं जिनका प्रभाव क्रमिक रूप से पड़ता है। भोजन का गुण अन्दर संचित हो जाने पर मन उसी गुण को प्रतिबिम्बित करने लगता है। यह और भी हानिकारक है; क्योंकि मन मायावी है। शराब आदि तो केवल तत्काल ही प्रभाव डालते हैं। अतः हमें भोजन के तीनों गुणों यथा सत्त्व, रजस् एवं तमस् में भोजन को वर्गीकृत करके ध्यान में रखना है कि सात्त्विक भोजन द्वारा ही आन्तरिक शुद्धि बनी रहती है।
बिना यह सोचे कि पदार्थ पवित्र है अथवा अपवित्र, उनका सेवन मत करो। क्यों? यहाँ भी एक महत्त्वपूर्ण नियम हमारे समक्ष है। 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन'- यह लोक-प्रसिद्ध सूत्र (वाक्य) है। एक और कहावत है- 'पवित्रता भगवान् का दूसरा स्वरूप है।' अपनी अधःतम अवस्था में हम शरीर के बन्धन में हैं। अतः हम कितना भी उच्चतम वेदान्तिक विचारों का आवाहन क्यों न करें, मूल-विचार तो यही रहता है कि मैं यह शरीर हूँ। जब तक हमारे जीवन में देह-भावना प्रधान है, तब तक हमें ध्यान रखना है कि शरीर का मन पर पड़ने वाला प्रभाव सुनिश्चित, ऊर्ध्वमुखी (उन्नति की ओर ले जाने वाला) एवं पावनता का वर्णन करने वाला हो। अतः मन पर होने वाले शरीर के प्रभाव का आग्रह है कि शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, जिससे मन भी शुद्ध रह सके। अपवित्र तत्त्वों के आने पर मन स्वभावतया ही एक प्रकार की प्रतिकूलता का अनुभव करेगा। यही है बाह्य एवं आन्तरिक शुद्धि। निश्चित रूपेण, योग में सदा अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। शुद्धता के नियम की सनक सवार नहीं होनी चाहिए। सहज बुद्धि का प्रयोग सर्वदा हितकर होता है, अन्यथा पथ-भ्रान्त होना पड़ेगा। साधक को सर्वदा स्वस्थ चित्त होना चाहिए।
एक अन्य तथ्य और सामने आता है। मन क्या सोचता है, इस बात को ध्यान में रखे बिना ही कर्म संयत करने से क्या लाभ? 'मन को स्वेच्छापूर्वक चिन्तन करने दो। मैं इसे अनुमति नहीं दूंगा कि यह मुझे कर्म करने के लिए बाध्य करे।' ग्रामवासियों में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जब तक सिंह अथवा किसी वन्य पशु ने मानव-रक्त का आस्वादन नहीं किया, तब तक वह मनुष्य से भय करता है और उसे कभी नहीं मारता। वह गाय, बकरी, भेड़ पर चाहे आक्रमण कर दे, पर मनुष्य पर नहीं करता। परन्तु वे कहते हैं कि एक बार भी मानव-रक्त का स्वाद ले लेने पर वह मानव-भक्षी बन जाता है। तब वह सदा मनुष्य पर आक्रमण करना आरम्भ कर देता है, उसे छोड़ता नहीं।
मन सहस्र सिंहों से भी बढ़ कर है। एक बार किसी कार्य-विशेष का चस्का पड़ जाये तो वह उसी का आदी हो जाता है। कर्म का चस्का एक क्षण में पड़ जाता है। अतः आपको जीवन-यापन की आदतों के सम्बन्ध में दृढ़ नियमों का पालन करना चाहिए। उनको व्यर्थ अथवा महत्त्वहीन समझ कर त्यागना नहीं चाहिए। वे योग के महत्त्वपूर्ण अंग हैं।
सन्तोष
नियम का अगला अंग है सन्तोष । इस विचार को सम्यक् रूप से ग्रहण करना कुछ कठिन-सा है। सन्तोष का अर्थ है तृप्त एवं प्रसन्न रहने की आदत। यह गुण अति-श्लाघनीय है। सन्तुष्टि अविरल आनन्द है। यह बहुत बड़ा गुण है। सन्तुष्टि क्या है, इसे वास्तविक रूप में समझना अत्यधिक कठिन है। कुछ लोगों का विचार है कि सन्तोष उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है; परन्तु यदि व्यक्ति में महत्त्वाकांक्षा बढ़ जाती है तो वह आगे और कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तथा और आगे उन्नति करता है। परन्तु उन्नति है क्या ? लौकिक व्यवहार में की गयी उन्नति हमें और बन्धन में डालेगी। यह संसार निस्सार होने के कारण त्यागने योग्य है। अतएव साधक की दृष्टि में ऐसी उन्नति का कोई मूल्य नहीं। वह मूल्य का भिन्न अर्थ लेता है। जिज्ञासु कहता है कि संसार के सुख-भोग में अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्म-साक्षात्कार की महत्ता संसार के सब सुख एकत्र कर लेने पर भी प्राप्त नहीं होती। कठोपनिषद् में नचिकेता द्वारा दिया गया उत्तर ही 'मूल्य' शब्द का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करता है। क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। नचिकेता ने पूछा था, 'क्या यह अविनाशी है, स्थायी है?' उसने कहा, 'मुझे ऐसे पदार्थ की कामना नहीं है जो केवल दो दिन रह कर समाप्त हो जाये। मुझे वह चाहिए जो शाश्वत है।' साधक यही सिद्धान्त ग्रहण कर लेता है और तब संसार के सब सुख व्यर्थ हो जाते हैं। संसार के सब पदार्थ नश्वर हैं। उसने (नचिकेता ने) सबको अस्वीकार कर दिया और कहा- मुझे वह सब नहीं चाहिए। यह साधक की मनोवृत्ति है। जो कुछ भगवान् ने आपको दिया है, उसी में सन्तोष करना चाहिए। 'भगवान् ने मुझे ऐसी नाक क्यों दी है?' इस प्रकार के विचार कभी मन में नहीं लाने चाहिए। जो आपके पास है, उसी में प्रसन्न रहिए।
जो पदार्थ आपके पास नहीं है; परन्तु दूसरों के पास है, आप सदा उसी का चिन्तन करते रहते हैं। आपको दुःखी बनाने के लिए यह मन की सबसे बड़ी चाल है। प्रदेश का प्रधान नायक सोचता है कि वह राजा बन जाये और राजा की इच्छा होती है कि वह चक्रवर्ती सम्राट् बन जाये एवं सम्राट् चाहता है कि वह सम्पूर्ण विश्व को जीत ले। मन की भिक्षा-वृत्ति कभी समाप्त अथवा सन्तुष्ट नहीं हो सकती। विश्व पर शासन करने वाला स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त करने की कामना करता है और यदि वह स्वर्ग का राजा इन्द्र भी बन जाये, तब कुछ और सोचने लगेगा। सृष्टिकर्ता के पद-पर्यन्त असन्तोष ही है। परन्तु फटे वस्त्र पहन कर भी यदि कोई सन्तुष्ट है तो वह प्रसन्न भी है। अतः जिस दशा में प्रभु ने आपको रखा है, उसी में सन्तुष्ट रहिए। आपमें कितनी ही योग्यता और बुद्धि-कौशल हो, आपके पास कितनी भी सम्पत्ति हो और कितनी ही दैनिक आवश्यकता हो, आप सन्तोष रखिए। यही सुख एवं शान्ति प्राप्त करने की कुंजी है।
एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात है-सन्तोष प्राप्त होने पर स्पर्धा-भाव नहीं रहता। वैसे तो आप सोचते हैं- 'उस मनुष्य के पास अमुक पदार्थ है, मेरे पास नहीं है।' परन्तु इसमें भी ईर्ष्या की भावना है। सन्तोष में सुख निहित है। उसमें स्पर्धा-भाव नहीं रहता। स्पर्धा-भाव से ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वन्द्विता एवं वैर-भाव उत्पन्न होता है। यदि आप उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते जो दूसरे के पास है तो आपका यह प्रयत्न रहता है कि किसी प्रकार वह व्यक्ति भी उस वस्तु से वंचित हो कर आपके स्तर पर पहुँच जाये। ईर्ष्या-भाव ऐसा ही होता है। यदि आप दूसरे व्यक्ति के स्तर पर नहीं पहुँच सकते तो आप उसे स्वतः निम्न स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। उसके प्रति आप कुछ बुरे प्रवाद फैलाने लगते हैं। यह सब भाव असन्तोष के कारण ही आते हैं। सन्तोष से मन की अद्भुत शुद्धि होती है। मन ईर्ष्या-भाव एवं क्षुद्रता से मुक्त हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मन की पवित्रता प्राप्त होती है। अतएव, निर्मलता प्राप्त कीजिए जो सन्तोष की प्राप्ति हेतु आवश्यक तथा पूर्वाकांक्षित गुण है।
सन्तोष साधना में नहीं होना चाहिए, उसमें आपको असीम असन्तोष होना चाहिए। आपको प्रभु के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए, न औदार्य आदि के विकास की मात्रा से। यही सोचना चाहिए कि मुझमें अभी तक अपूर्णता है। भक्ति कहाँ है? स्वयं की सदा उन महान् आत्माओं से तुलना करनी चाहिए जिन्होंने प्रभु के वियोग में व्यथा का अनुभव किया है। इनमें चैतन्य महाप्रभु, रामलिंग स्वामी आदि के नाम स्मरणीय हैं। प्रभु के लिए उनकी वेदना इतनी अधिक थी कि स्वयं प्रभु को दर्शन देना ही पड़ा। वे दर्शन देने से इन्कार नहीं कर सके। अतः आध्यात्मिक क्षेत्र में उपलब्धि से आपको सदा असन्तुष्ट रहना चाहिए।
तप
तपस्या क्या है, इससे सम्बद्ध अनेक धारणाएँ हैं जिनमें कुछ अज्ञानजनित एवं अयुक्त हैं। कुछ लोगों का विचार है कि यदि कोई व्यक्ति एक पाँव अथवा एक हाथ ऊपर उठा कर खड़ा रहे तो वह तपस्या है। शीत-ऋतु में ठण्ढे पानी में खड़े रहना, शीर्षासन में खड़े रहना, स्वयं को पृथ्वी में गड़वा देना आदि ऐसे कुछ कार्य तप के रूप में माने जाते हैं। परन्तु प्रश्न है कि तपस्या क्या है? इसका आन्तरिक स्वरूप क्या है? इस प्रश्न को प्रत्येक जिज्ञासु को समझना चाहिए। तप का योग में क्या स्थान है और इसका क्या अर्थ है, इन बातों से अनभिज्ञ रह कर साधक मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं।
तप का मूलार्थ है जलना, दहन करना। तप शब्द उष्णता का अर्थ प्रतिपादित करता है और इस प्रकार कुछ प्रचण्डता का बोधक-सा प्रतीत होता है। तपस्या या प्रचण्डता-इसका अर्थ क्या है? अग्नि में पवित्र करने की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। यह पदार्थों को प्रकाशित भी करती है। अग्नि के ये दो लक्षण सदा स्मरण रखने चाहिए। यह मल को जला कर पदार्थ में शुद्धता लाती है और तेजयुक्त है। अतएव वास्तव में तपस्या एक प्रचण्ड प्रक्रिया है जो मानव-मन के मलों को जला कर उसे पावन आत्म-चैतन्य के प्रकाश से उद्भाषित करती है। तपस्या का मुख्य कार्य यही है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व की पवित्रता एवं उज्ज्वलता है। विभिन्न व्यक्तियों के लिए तप का अर्थ भिन्न हो सकता है। आत्म-शुद्धि के लिए आपको एक प्रकार के तप की आवश्यकता है तो दूसरे व्यक्ति को किसी अन्य प्रकार के तप की आवश्यकता है; क्योंकि भोग-विलास-रूपी अशुद्धि अन्यान्य व्यक्तियों में भिन्न हो सकती है।
तो, तपस्या का कोई सार्वलौकिक रूप नहीं है; परन्तु फिर भी इसके कुछ सर्वसाधारण रूप हैं; क्योंकि सर्वसाधारण में पायी जाने वाली कुछ दुर्बलताएँ सामान्य हैं। अधिकांश लोग पेटू होते हैं और बहुत अधिक भोजन करते हैं। अतएव निराहार रहना सर्वमान्य तप है। आत्म-संयम के लिए, धार्मिक व्रत एवं तपश्चर्या करने के लिए तथा वीतराग बनने के लिए निराहार व्रत सब साधु-सन्तों, साधकों, जिज्ञासुओं एवं रहस्यवादियों में सामान्यरूपेण प्रचलित है। कामोत्तेजना, आसक्ति अथवा सम्भोग की दुर्बलता भी सार्वलौकिक दुर्बलता है। इसलिए सब साधकों के लिए ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत ले लेना भी तपस्या का ही एक सामान्य रूप है। मन के अशुद्ध उद्वेगों और भावों को नियन्त्रित करना भी बहुत बड़ी समस्या है। स्वभाव-शुद्धि का इससे उत्तम कोई उपाय नहीं है।
तपश्चर्या इन्द्रियों को संयत करने और आन्तरिक शुचिता की आग को प्रज्वलित करने के लिए है। तपस्या की बाह्य विधियों के सम्बन्ध में तप के परोक्ष ढंग हैं। यदि कोई सोचे कि बिना कुछ खाये-पीये चौबीस घण्टे खड़ा रहना तपस्या है तो यह गलत है। तमोगुणी प्रकृति वाले पुरुष के लिए ऐसी तपस्या लाभकारी हो सकती है। कृतसंकल्प के लिए अपार शक्ति की आवश्यकता है। तमोगुण है आलस्य एवं तन्द्रा। आराम चाहने वाला कदापि साधक नहीं बन सकता। अतः इस पर विजय पाने के लिए यदि आप कुछ उग्र संकल्प कर लें, जैसे कि काया को अरुचिकर कार्य करने के लिए बाधित करना, जिसे आप अपनी इच्छा के बल पर करते हैं और इस प्रकार अपने स्वभाव पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं-इनसे कुछ लाभ-प्राप्ति हो सकती है; परन्तु लक्ष्य यह नहीं है।
निराहार रहने के लिए निराहार रहना आपका लक्ष्य नहीं है। जिन पदार्थों को आप अत्यन्त रुचिकर समझते हैं, उन्हें माह में एक बार त्यागना, नवरात्रि आदि में नमक का त्याग करना, सात दिनों तक चाय-पान न करना-ये सब बौद्धिक अनुशासन द्वारा अधम प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के कुछ साधन हैं। मन एवं इन्द्रियों पर विवेकयुक्त बुद्धि का प्रयोग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु जो आपकी प्रकृति को शुद्ध करती है और आपको ब्रह्म-भावना से भरती है, तपस्या कहलाती है। मन एवं इन्द्रियों पर किसी प्रकार का भी संयम तपस्या है।
एक बार देवताओं की सभा में एक विवाद उत्पन्न हुआ। कुछ बोले, "शीत काल में शीतल जल से स्नान करना, रुक्ष वस्त्र धारण करना और कायिक विरक्ति श्रेष्ठतम हैं।" कुछ अन्य देवताओं ने कहा, "नहीं, कलियुग में सत्य तपस्या से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यदि आप सत्यनिष्ठ बने रहें तो भगवान् स्वयं आपके समक्ष प्रकट होंगे। नितान्त सत्यनिष्ठ को ही ईश्वर-प्राप्ति होगी। राजा हरिश्चन्द्र, युधिष्ठिर, मार्कण्डेय आदि सत्य के ही पुजारी थे।" तदुपरान्त गहन वाद-विवाद आरम्भ हो गया।
उन्होंने निश्चय किया कि भू-लोक में जा कर ज्ञानी पुरुषों की सम्मति ली जाये। वे सब नैमिषारण्य पहुँचे। वहाँ योगी गण आध्यात्मिक विषयों पर परिचर्चा कर रहे थे। उन्होंने ऋषियों से पूछा, "तपस्या एवं सत्य में श्रेष्ठ कौन है?" ऋषियों ने तत्काल उत्तर नहीं दिया। उन्होंने परस्पर विचार-विमर्श किया और यह कह कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया कि दोनों ही श्रेष्ठतम हैं। तदुपरान्त उन्होंने व्याख्या दी, "इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ तपस्या सत्यनिष्ठा है।" यदि कोई मनुष्य सत्यनिष्ठ होने का प्रयत्न करे तो उसे प्रतीत होगा कि कौन-कौन से अनुभवों एवं परीक्षाओं से उसे गुजरना पड़ता है। परम सत्य को अपनाने पर व्यक्ति को सर्वस्व खो कर कठोरतम अनुभवों एवं दुःखों का सामना करना पड़ सकता है। अतः उन्होंने कहा कि सत्य ही महान् तपश्चर्या है।
ऐसा निर्णय देने का उनका अभिप्राय यही था कि जो कुछ भी आपको सत्य के और समीप लाये, वही सर्वोत्तम तपश्चर्या है। इसका कोई भी रूप हो सकता है, कोई निश्चित रूढ़िगत रूप नहीं है। मानव-इन्द्रियों पर संयम तप है। अधम प्रकृति, कामासक्ति पर विजय पाने के लिए दृढ़ निश्चय से किया हुआ कोई भी कार्य तपश्चर्या का सारतत्त्व है। ऐसी तपस्या आपकी दुर्बलता को दूर करेगी। यदि आप अपनी साधना के प्रति सत्यनिष्ठ एवं संकल्पचित्त हैं तो आपके जीवन का प्रत्येक क्षण तपस्या बन जायेगा।
स्वाध्याय
नियम का चतुर्थ अंग है स्वाध्याय अर्थात् आध्यात्मिक एवं धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन जो आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म, दिव्य जीवन यापन एवं दिव्य जीवन के ज्ञान के प्रेरणा-स्रोत हैं। यह ज्ञान सब सम्प्रदायों के समस्त धर्मशास्त्रों में निहित है। इनमें ब्रह्मज्ञानी महर्षियों का वह ज्ञान संचित है जो भौतिक पदार्थों के ज्ञान से कहीं उच्च है। ऋषियों द्वारा ध्यान एवं समाध्यावस्था में प्राप्त सब अनुभव, रहस्योद्घाटन एवं गूढ़ आन्तरिक ज्ञान उपनिषद् आदि धर्मग्रन्थों में दिये गये हैं। इनमें पुरातन ऋषियों के दिव्य अनुभवों के लेख अंकित हैं, जिन्होंने दृढ़ निश्चय द्वारा ज्ञान के नित्य-स्रोत तक पहुँच कर स्वयं को उच्चतर आध्यात्मिक लोक में अधिष्ठित किया। उन्होंने इन शास्त्रों में एवं इनके द्वारा ज्ञान का प्रसार किया। इन ग्रन्थों में उच्च कोटि के शाश्वत ज्ञान का विवरण मिलता है। इन ग्रन्थों में दिये हुए सन्देश सदा-सदा के लिए कल्याणकारी हैं। उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। उन सन्देशों में नश्वर पदार्थों की चर्चा नहीं है। लौकिक पदार्थों का ज्ञान परिवर्तित होता रहता है; क्योंकि पदार्थ ही परिवर्तनीय हैं; परन्तु परम सत्य नित्य है, अद्वितीय है और इसका ज्ञान भी शाश्वत है। इसलिए उन शास्त्रों में आचक्षित मूल सत्य में विविधता नहीं हो सकती। वे सार्वकालिक सत्य हैं। उत्तर काल में अन्य महर्षियों द्वारा इन शास्त्रों पर व्याख्या दी गयी और इन्हें विस्तृत किया गया है। मूल सत्य के विभिन्न रूप, जिनका अनुभव रहस्यवादियों ने अपने जीवन में किया, विस्तृतरूपेण बताये गये हैं।
भारत में अनेक अवतार हुए एवं सबने देश के विभिन्न भागों में अपने ग्रन्थों को प्रदान किया। यही वह ज्ञान का कोष है जिससे हम स्वाध्याय के द्वारा मार्ग-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय उन्नत, उत्कृष्ट एवं जीवन में दिव्यान्तर लाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान के विशाल कोष की कुंजी मात्र है। धर्मशास्त्रों के स्वाध्याय से दिव्य जीवन व्यतीत करने तथा भौतिक जीवन से ऊपर उठने का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। इससे सदाचार का, आध्यात्मिक जीवन का रहस्य ज्ञात होता है। विश्वविद्यालयों की पाठ्य-पुस्तकों में यह ज्ञान नहीं मिलता। अन्तर के दिव्य तत्त्व को कैसे जागृत किया जाये और आध्यात्मिक मार्ग में क्रमशः कैसे उन्नति की जाये, यह सब ज्ञान विधि, चिकित्सा अथवा व्यवसाय-सम्बन्धी पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा की शाश्वत नियति का निर्माण करने के लिए आपको कालेज की पाठ्य-पुस्तकों और जिनसे सर्वसाधारण पुस्तकालय भरे पड़े हैं, ऐसी पुस्तकों को छोड़ अन्य ग्रन्थों की शरण में जाना है। आपको अध्यात्म-सम्बन्धी पुस्तकें तथा सन्तों की जीवनियों का अध्ययन करना है जिनके अन्तर में जीवन का सत्य है, सत्य-रूपी माणिक्य है। और इसीलिए स्वाध्याय एक स्वर्ण-कुंजी है जो हमारे लिए ऐसे नित्य-ज्ञान का, अध्यात्म-ज्ञान का कोष खोलती है जो साधक के पूर्णता और अमरत्व-पथ का प्रदर्शक है। यही स्वाध्याय का माहात्म्य है।
अब हमें देखना है कि स्वाध्याय का मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक महत्त्व क्या है तथा स्वाध्याय से जीवन में क्या प्राप्त किया जा सकता है? इसका अत्यन्त गूढ़ एवं युक्तियुक्त कारण है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वे संस्कार का रूप धारण कर लेते हैं तथा मन पर अपने चिह्न छोड़ जाते हैं। ये चिह्न बीज का रूप ले लेते हैं और यह तो आप जानते ही हैं कि मन की प्रकृति, जो वासना मन ग्रहण करता रहता है, उसके अनुसार परिवर्तित होती है। इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए महर्षियों ने कहा है कि यदि मानव उन्नति करना चाहता है और सब अवांछित वासनाओं का अतिक्रमण करना चाहता है तो व्यावहारिक जीवन में बनने वाली मानसिक वासनाओं को दूर करने के लिए कुछ उपायों का निरूपण किया जाना चाहिए। इन वृत्तियों को बदलने अथवा नष्ट करने के लिए उन्होंने हमें स्वाध्याय प्रदान किया है।
स्वाध्याय कुछ इस प्रकार कार्य करता है। मान लीजिए, आप एक लकड़ी के तख्ते में कील ठोकते हैं और तभी आपको पता चलता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी तो उस कील को निकालने के लिए आप उस स्थान पर दूसरी कील ठोकने लगते हैं। इस प्रकार पहली कील स्वतः बाहर आ जाती है और दूसरी कील काष्ठ-फलक में चली जाती है। लगभग इसी भाँति, प्रतिदिन एक-एक वासना को दूर करने का यत्न करने की अपेक्षा, जिसमें आपकी स्नायविक शक्ति भी बहुत अधिक लगती है, आप स्वाध्याय करें। प्रतिदिन प्रातः-सायं आप अतीत के विभिन्न युगों के दिव्य महापुरुषों से (अनुशीलन द्वारा) सम्पर्क स्थापित करें जिनके वचन, उनके निजी अनुभवों से उत्पन्न होने के कारण प्रभावशाली हैं। वे आपकी काया-पलट करने वाले वचन हैं। अतः आप इन विगत युगों के महामना महापुरुषों से सीधा सम्पर्क स्थापित करें जिनके जीवन्त अनुभवों से धर्मशास्त्रों के पृष्ठ भरे पड़े हैं। धर्मशास्त्र का अध्ययन करते समय आप भौतिक लोक से ऊपर उठ कर अनुभव से उद्भूत विचारों के एक नये (अनुभव से उद्भूत) लोक में प्रवेश करते हैं। इन ग्रन्थों में उनके निर्माता महर्षियों के आध्यात्मिक आलोक की दीप्ति भी है।
अतः स्वाध्याय का अर्थ है शंकराचार्य, ईसा मसीह जैसे अध्यात्म शास्त्रों के रचयिताओं के समक्ष बैठना। यह भी एक प्रकार का परोक्ष सत्संग है। जब आप स्वाध्याय के लिए बैठते हैं तो स्वयं को उन महान् आत्माओं के ध्यान में निमग्न कर दें जो साक्षात्कार के आलोक से उद्भासित हैं। ये महापुरुष सदा अमर हैं। उनका नाश नहीं हुआ। उनका अस्तित्व लोप नहीं हुआ। वे परमात्मा के साथ एक-रूप हो गये हैं और इसीलिए उनका व्यक्तित्व भी अमर है। वह कभी नष्ट नहीं होता। उनका अस्तित्व साधारण व्यक्ति के अस्तित्व की तरह नहीं है, जो प्रत्येक मृत्यु के उपरान्त नया रूप धारण करता है। अतः आप उन महर्षि गण से सम्पर्क स्थापित करें जो अदृश्य रूप में वर्तमान हैं।
प्रबुद्ध पुरुषों की पुस्तकें पढ़ कर आप उनकी संगति प्राप्त करते हैं। सभी लोग महात्माओं का सत्संग नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ ही लोगों को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। अतएव, सन्तों से व्यक्तिगत रूप से मिल कर आपको उनसे अधिक-से-अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। तदुपरान्त, स्वाध्याय द्वारा आपको स्वयं लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप 'हिमालय के अंचल से' (Voice of the Himalayas) पुस्तक पढ़ें तो आप अनुभव करेंगे कि आप स्वामी शिवानन्द जी महाराज के साथ हैं और वे आपसे बातें कर रहे हैं। लेखक तो अनेक हैं। साधारण लेखक भी, जिनमें आत्म-शक्ति नहीं है, प्रेरणा देने में सफल हो गये हैं। जब साधारण लेखक भी ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है तो उन लेखकों का कहना ही क्या जो आत्मवादी हैं, जिनका प्रत्येक शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित है? उनका अनुभव गहन है। वे पाठक की भावुकता एवं उसके मानसिक स्तर पर ही आधिपत्य नहीं जमाते, अपितु प्रतिदिन नियमपूर्वक स्वाध्याय करने वाले के आत्म-तत्त्व को भी स्पर्श करते हैं। प्रतिदिन का स्वाध्याय ज्ञान-गंगा में डुबकी लगाने के समान है। स्वाध्याय द्वारा आप आध्यात्मिक स्नान करते हैं, आप सदा व्यावहारिक विचारों के सागर में डूबे रहते हैं। अक्षर सन्तों की संगति कीजिए और उनके सद्वचनों से प्रवाहित ज्ञान-सागर में डुबकी लगाइए। स्वाध्याय यही कराता है।
उपनिषद् कहते हैं : 'स्वाध्यायान्मा प्रमदः' - स्वाध्याय की उपेक्षा न करो। ऋषि-मुनियों ने हमें स्वाध्याय की यह अमूल्य प्रक्रिया प्रदान की है जिससे कि हम महामना महात्माओं से सम्पर्क स्थापित कर सकें। स्वाध्याय का मुख्य उद्देश्य यही है। स्वाध्याय करते समय यदि आप पुस्तक-विशेष में खो जायें तो आपके विचार पूर्णतया दिव्य भाव में आबद्ध हो जायेंगे। संज्ञान युक्त यह भी एक प्रकार की सविकल्प समाधि है; क्योंकि उस समय मन सब सांसारिक विचारों से रिक्त हो कर आध्यात्मिक विचारों में समाहित हो जाता है। निरन्तर स्वाध्याय करते रहने से क्या होता है? जो विचार आप मन में धारण कर लेते हैं, उनसे प्रेरणाप्रद भाव जागृत होते हैं और आपका मन सात्त्विक विचार-रूपी सम्पत्ति से भर जाता है। स्वाध्याय में प्रतिदिन आपको उद्बुद्ध, उच्चतर एवं प्रेरणादायक आध्यात्मिक विचार मिलते हैं जिनसे निराशा के क्षणों में आपको शक्ति प्राप्त होती है। अनुमान करें कि आप निराश हैं तो स्वाध्याय आपका उत्थापन करता है, तेज प्रदान करता है और आत्मा को दैनिक आध्यात्मिक भोजन प्रदान करता है। आत्मा के लिए आप यही भोजन करते हैं।
प्रातःकाल से ले कर सायंकाल तक आप व्यवहार करते हैं। अनन्त बिचार और संस्कार उत्पन्न होते हैं। अतः सायंकाल को आपको स्वाध्याय करना चाहिए जिससे सब असात्त्विक एवं लौकिक संस्कार दूर हो जायें। उन्हें ठहरने का अवसर न दें। अतएव, स्वाध्याय का एक व्यावहारिक लाभ यह है कि इससे मनुष्य सात्त्विक विचार ग्रहण करता है और वे सांसारिक विचारों को आच्छादित कर लेते हैं। दूसरा लाभ है स्वाध्याय मन को एकाग्र करने तथा ध्यान लगाने के लिए भी सहायक है। परन्तु कैसे ? एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है। हमारा उद्देश्य अथवा प्रयत्न तो यही होता है कि मन किसी एक ही सुविचार में अवस्थित रहे। प्रार्थना और पूजा का भी यही भाव है जिससे कि अन्ततः मन एक ही विचार में निमग्न रह सके; परन्तु मन सर्वदा अवांछित पदार्थों के विषय में सोचता रहता है।
साधारण अपरिष्कृत मनुष्य का मन अनेक प्रकार की काम एवं विषय-वासनाओं से युक्त होता है। समस्त चिन्तन विषयों की तुष्टि के सम्बन्ध में, सांसारिक पदार्थों के सम्बन्ध में होता है। मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं कि जो वह सूँघता अथवा स्पर्श आदि करता है, इनके आगे भी कोई सत्ता हो सकती है। परन्तु यह ज्ञात होने पर कि यह सब विचार वास्तविक विकास एवं उत्थान के लिए नहीं हैं, मन अच्छे विचार ग्रहण करने का यत्न करता है। कभी बुरे (असात्त्विक) विचार मन में आते हैं तो कभी अच्छे (सात्त्विक)। यह मन तो एक मक्खी की भाँति है जो कभी तो अच्छे पदार्थों पर बैठती है और कभी थूक पर भी बैठ जाती है। इस प्रकार, मन अन्यान्य पदार्थों में विकल्पित रहता है; परन्तु मधुमक्खी सदा फूलों पर ही बैठती है, गन्दगी पर नहीं; इसी भाँति मन को मक्खी की प्रथमावस्था से विमुख करके मधुमक्षिका की द्वितीयावस्था में ला कर, अन्ततः इसे उच्चतर अवस्था में स्थिर करना है। स्वाध्याय का यही कार्य है। इससे मन केवल उत्कृष्ट विचारों की ओर ही प्रेरित होता है और असात्त्विक विचारों के लिए मन में स्थान नहीं रहता। जिसका चिन्तन करने को बारम्बार मिले, मन उसी को ग्रहण करता है। आरम्भ में तो मन विरोध करेगा, परन्तु तत्पश्चात् आनन्द मिलने पर स्वाध्याय के बिना आपको भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। यह मनुष्य-जीवन का एक आवश्यक अंग है। यह आत्म-सत्ता का भोजन है। ऐसी आदत पड़ने पर मानस पटल पर केवल सात्त्विक विचार ही हावी हो जाते हैं। स्वाध्याय की यह गूढ़, आन्तरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्रिया-प्रणाली है।
मान लें, घुड़दौड़ के एक घोड़े की कीमत पन्दरह लाख रुपये है। उसका स्वामी घोड़े को इधर-उधर जाने और हर तरह की चीजें खाने की आज्ञा नहीं देगा। उसे चुना हुआ भोजन ही दिया जायेगा। मन भी एक अत्यन्त अमूल्य अश्व की भाँति है। यह हमें परम धाम, ब्रह्मपुरी पहुँचायेगा। यदि स्वामी इतस्ततः घूमने देना नहीं चाहता तो वह उसके लिए अच्छी घास ले कर आयेगा। फिर अश्व को घास के पास ले जा कर खूंटे से बाँध देगा। यहाँ अश्व को कुछ स्वतन्त्रता होती है, परन्तु यह सीमित है। यदि रस्सी बीस मीटर लम्बी है तो वह चालीस मीटर व्यास के भीतर ही घूम सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यद्यपि वह बँधा हुआ है, पर उसे स्वतन्त्रता है कि उस सीमित क्षेत्र में से वह कुछ भी लेना चाहे तो ले ले। स्वाध्याय भी यही करता है। नियमपूर्वक स्वाध्याय करने पर मन में एक नवीन चरागाह-सा बन जाता है। पहले तो मन मनचाहा घूमता था, परन्तु अब उसे भोजन के लिए (स्वाध्याय के रूप में) सीमित एवं सुचारु पदार्थ उपलब्ध हो गये हैं। निरन्तर स्वाध्याय में लगे रहने से मन आध्यात्मिक पुस्तकों के ही विचार ग्रहण करने लगता है। वह इस सीमा से परे नहीं जाता और स्वाध्याय का आदी हो जाता है। यह स्वाध्याय का दूसरा रूप है जिसे प्रत्येक जिज्ञासु को जानना चाहिए।
स्वाध्याय एक प्रकार का परोक्ष सत्संग है। महापुरुषों द्वारा आचक्षित शाश्वत ज्ञान के क्षेत्र में यही पहुँचाता है। इससे हमें महापुरुषों के साथ आध्यात्मिक एकरूपता प्राप्त होती है और मन को भोजन हेतु नवीन क्षेत्र प्राप्त होता है। मन में आने वाले बुरे संस्कारों के लिए यह बन्ध-स्वरूप है।
ईश्वर-प्रणिधान
ईश्वर-प्रणिधान 'नियम' का पाँचवाँ महत्त्वपूर्ण अंग है। नियमों में यह सर्वोच्च है। ध्यान रखिए कि ये यम-नियम आध्यात्मिक जीवन के प्रथम चरण मात्र हैं; किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि किसी भी समय आध्यात्मिक प्रयत्नों में इनको अनावश्यक माना जा सकता है। यम-नियम का अभ्यास करने के पश्चात् ही धारणा का अभ्यास किया जाता है। परन्तु यम-नियम का पालन भी साथ ही करना पड़ता है। उसका त्याग नहीं किया जाता। जब आप भवन-निर्माण कर रहे हैं तो आप नींव नहीं हटा सकते। जब तक आत्म-दर्शन नहीं होता, तब तक यम-नियम का पालन निरन्तर करना चाहिए। साक्षात्कार होने के उपरान्त साधक को यम-नियम के पालन की आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि तब ये उसके स्वभाव के अंग बन जाते हैं। सात्त्विकता ही उसकी प्रकृति बन जाती है। सिद्ध योगी के कर्मों से यह स्वतः ही प्रकट हो जाता है। नृत्य सीखते समय कदमों पर ध्यान देना अनिवार्य होता है; परन्तु नृत्य में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लेने पर इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती और तब उसके विषय में सोचना भी अनिवार्य नहीं; क्योंकि गलत कदम उठेगा ही नहीं। ऐसी अवस्था प्राप्त होने तक अभ्यास अनिवार्य है। ईश्वर-प्रणिधान का अर्थ है स्वयं को ईश्वर में प्रतिष्ठित कर देना अर्थात् सदा आत्म-तत्त्व की प्रत्यक्षता में निवास करना। परन्तु यह कहाँ फलित होता है? एक अधम पुरुष भी देवता के समक्ष नम्र हो जाता है। उसका आचार-व्यवहार ही बदल जाता है। अपने से उच्च शक्ति के सामने आ कर आप स्वयं को निम्न समझने लगते हैं। ईश्वर-प्रणिधान का अर्थ है पूजा, भक्ति, विश्वास (आस्था) एवं नम्रता को निरन्तर जीवन में चरितार्थ करना। ईश्वर के सान्निध्य के भाव में निरन्तर रहने से अहं-भाव दूर होता है। अहंकार को वश में करने के लिए यह प्रभावपूर्ण उपाय है। इससे भाव पूजा एवं भक्तिमय बनते हैं तथा प्रभु से मिलन सुसाध्य हो जाता है। ईश्वर-प्रणिधान का अन्तिम लक्ष्य आत्म-दर्शन है।
ये उपाय योग के विभिन्न स्वरूप ही हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता में विश्वास करने वाले व्यक्ति के सब कर्म स्वतः ही संयत हो जाते हैं। ईश्वर की विद्यमानता में वह कोई दुष्कर्म नहीं कर सकता। स्वयं को बाह्य एवं आन्तरिक सम्पूर्ण रूप से प्रभु को अर्पित करने से मन, वचन और काया से सभी कर्म स्वतः ही पुण्यशील, निर्दोष एवं पूर्ण होने लगते हैं। विमलात्मा हो कर सच्चे हृदय से प्रभु को ही सर्वत्र देखने का अभ्यास साधक को शनैः-शनैः प्रभावित करने लगता है। ऐसी अवस्था में किसी भी क्षण कोई भी कर्म करने पर विश्व-साक्षी ईश्वर की विद्यमानता का आभास होता है। तब साधक सावधान रहता है और कोई भी दुष्कर्म नहीं करता। उसके मन में भाव उठता है- 'मैं मरणशील मनुष्य से तो कुछ भी छिपा सकता हूँ; परन्तु परमात्मा से नहीं, इसलिए उसके सामने मुझे कोई दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए।' किसी को मिठाई दे कर आदेश दिया जाता है- 'जाओ, और इसे ऐसे स्थान पर खाओ जहाँ देखने वाला कोई न हो।' वह व्यक्ति वापस चला आता है और मिठाई को वापस करते हुए कहता है- 'मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं दिखायी देता जहाँ परमात्मा न हो।’
श्रीमद्भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय के भाव को समझने और ग्रहण करने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति के मन में प्रभु की सर्वव्यापकता का भाव स्वतः ही आने लगता है।
इस अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं- "मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करूँगा जिससे तुम मेरे अनन्त स्वरूप के दर्शन कर सको।" वे अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और अपना विश्व-रूप दिखाते हैं। अर्जुन जिस ओर भी देखते हैं, उन्हें भगवान् ही दिखायी देते हैं। सब लौकिक पदार्थों में, चर-अचर में सर्वत्र उन्हें प्रभु की व्यापकता ही दृष्टिगोचर होती है और यह विश्व-रूप-दर्शन ही मोक्ष-प्राप्ति की कुंजी है।
प्रह्लाद के जीवन से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। उसने नारायण को ही सर्वत्र देखा। उसके पिता अत्यन्त क्रूर एवं नास्तिक थे। प्रह्लाद को माता के गर्भ में ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गयी थी। उसने सर्वत्र नारायण को ही देखा। नारायण के अतिरिक्त उसे और कुछ दिखायी नहीं देता था। अन्ततः पिता ने जब उससे पूछा, 'भगवान् कहाँ हैं?' उसने उत्तर दिया, 'आप मेरे से पूछ रहे हैं कि भगवान् कहाँ हैं। पूछना तो यह चाहिए कि वह कहाँ नहीं हैं।' तो पिता ने यह पूछते हुए, 'क्या वे इस स्तम्भ में हैं' क्रोध से स्तम्भ पर पादाघात किया। तत्काल ही स्तम्भ फट गया। उसमें से भगवान् नारायण नृसिंह के रूप में बाहर निकल आये और हिरण्यकशिपु का नाश कर दिया। प्रह्लाद के जीवन से हमें यह मुख्य शिक्षा मिलती है कि भगवान् सर्वत्र विद्यमान हैं। सम्पूर्ण विश्व उन्हीं से व्याप्त है। यत्र-तत्र-सर्वत्र भगवान् ही भगवान् हैं। जिस प्रकार मक्खन समस्त दूध में समाया रहता है उसी प्रकार भगवान् सम्पूर्ण विश्व में समाये हुए हैं। भगवान् की सर्वव्यापक प्रकृति का अविरत स्मरण आत्म-साक्षात्कार के मार्ग में कभी बाधा नहीं डालता। योग में समाधिस्थ होने के लिए यह सर्वोत्तम एवं निश्चित विधि है। अन्ततः योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, योग की अतल गहराइयों में प्रभु-मिलन का प्रयत्न। सभी महात्माओं ने यही शिक्षा भिन्न-भिन्न रूपों में देने का यत्न किया। जब नामदेव रोटी बना रहे थे तो एक श्वान आया और रोटी छीन कर ले गया। वे श्वान के पीछे घी ले कर यह कहते हुए भागे, "तुम्हारा गला खराब हो जायेगा। रोटी सूखी है, अतः घी ले लो।"
एक और कहानी इस प्रकार है। एक साधु तीर्थयात्रा करने के लिए वाराणसी गया। उसने वहाँ से गंगा जल लिया। साधारणतया लोग वाराणसी से गंगा-जल रामेश्वरम् ले जाते हैं जहाँ भगवान् शिव का मन्दिर है। वह भी जल ले कर रामेश्वरम् जा रहा था। बहुत दिनों की यात्रा के उपरान्त वह रामेश्वरम् के मन्दिर के समीप पहुँचा। गर्मी का दिन था। धूप प्रखर थी। मन्दिर के समीप ही एक गधा धूप में व्याकुल पड़ा था। वह गिर गया था और प्यास के कारण मरणासन्न हो रहा था। किसी के पास उसे देखने का समय नहीं था; परन्तु यह भक्त प्रभु की सन्निधि (प्रत्यक्षता) का अनुभव कर रहा था। गधे के समीप जाने पर उसने विचार किया कि जब साक्षात् भगवान् ही मेरे समक्ष हैं तो गंगा-जल का इससे अच्छा उपयोग क्या किया जा सकता है। उसने वह जल गधे के मुख में डाल दिया। उसने अनुभव किया कि साक्षात् भगवान् को ही वह गंगा-जल अर्पित कर रहा है और जिस देवता की अर्चना मन्दिर में अन्य लोग कर रहे हैं, वह देवता ही उसे आशीर्वाद दे रहे हैं।
एक बार जब स्वामी विवेकानन्द केदार-बद्री आदि की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने हिम-प्रदेश में एक साधु को पड़े हुए देखा। उन दिनों यात्रा के साधन आधुनिक समय से सर्वथा भिन्न थे। उस समय कोई सीधा मार्ग एवं उचित सुविधाएँ उपलब्ध न थीं। बड़ी कठिनाई से वे अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे थे। उन्होंने अपने मार्ग में ही हिम-प्रदेश में उस असहाय साधु को देखा। स्वामी विवेकानन्द जी ने अपना कम्बल उसे दे दिया। साधु ने विवेकानन्द पर दृष्टिपात किया और यह देख कर कि वह एक आत्मज्ञानी हैं, उसने अपने अतीत जीवन की कहानी आरम्भ की। उसने स्वामी विवेकानन्द से पूछा, "क्या आपने सन्त पवहारी बाबा का नाम सुना है?" तदुपरान्त उसने पवहारी बाबा के साथ हुई अपनी घटना का वर्णन किया और कहने लगा, "मैं एक डाकू था। जबसे उस सन्त से मेरा सम्पर्क हुआ, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। मैंने बहुत पश्चात्ताप किया। तभी से मैं अपने पापों का प्रायश्चित्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।"
तो यह है साधु-सन्तों की शक्ति। ईश्वर सर्वत्र हैं-केवल यही भाव तथा सबको मुक्ति की ओर अग्रसर कर सकता है; जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकता है।
आसन
यम और नियम के अभ्यास से मनुष्य की अन्तः तथा बाह्य प्रकृति की शुद्धि होती है और वह उच्चतर अनुभव प्राप्त करने योग्य हो जाती है। कायिक सारतत्त्व का ज्ञान भी तभी अर्थात् इनके अभ्यास के पश्चात् ही प्राप्त हो सकता है। यह तृतीयावस्था है। इसमें प्रविष्ट होने से पूर्व मानव-रचना के सम्बन्ध में कुछ गहरा ज्ञान होना आवश्यक है।
यह शरीर पाँच तत्त्वों से बना हुआ है। इसमें अदृश्य, शीघ्रगामी विद्युत् अणु विद्यमान हैं। प्रोटोन्स और इलेक्ट्रोन्स इस भौतिक शरीर के अत्यन्तरस्थ भाग हैं और विश्व की समस्त वस्तुएँ सत्त्व, रजस् तथा तमस्, इन तीनों गुणों से बनी हैं। ये तीन विविध स्पन्दन हैं जो भिन्न-भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। स्थूलतम क्रिया तमस्-प्रधान, सूक्ष्मतर क्रिया रजस्-प्रधान एवं सूक्ष्मतम क्रिया सत्त्व-प्रधान होती है।
राजयोग के तृतीय अंग आसन का उद्देश्य है इस काया को पूर्णतया सत्त्वगुण-प्रधान बनाना, प्रत्येक पदार्थ को सत्त्वगुण से समन्वित करना। महर्षि पतंजलि ने आसन का अनुष्ठान इसीलिए बताया है। यह आसन हठयोग में किये जाने वाले आसनों hat H सर्वथा भिन्न है। राजयोग के तृतीय अंग आसन में जहाँ तक पूर्ण दक्षता एवं सात्त्विकता का प्रश्न है किसी भी प्रकार की कायिक बाधा, कम्पन या गति की मन पर प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही है। शरीर और मन का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। वे एक-दूसरे पर आधारित रहते हैं। यदि आप शरीर को तीव्र झटके देंगे तो प्राण पर उसका प्रभाव होगा और प्राण का मन पर प्रभाव पड़ेगा।
अतः महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन का अभिप्राय है दीर्घ काल तक स्थिर एवं शान्त मुद्रा में शरीर को संयत रखना। सर्वथा निश्चल होने पर शनैः-शनैः श्वास भी संयत होने लगता है। श्वास भी नियमित हो जाता है। स्थिरतापूर्वक सुखासन में बैठा जा सकता है। यदि आसन सुखदायी न हो तो इसे बदल लेना आवश्यक है। ऐसे ही आसन में बैठना चाहिए जिसमें आपको कष्ट न हो और आप अधिक समय तक सुखपूर्वक बैठ सकें।
"स्थिरसुखमासनम्"-आसन वही है जो स्थिर और सुखदायी है। स्थिर एवं सुखदायी आसन ही सर्वथा निश्चल हो सकता है। दीर्घ काल तक ध्यान लगा कर बैठने की क्षमता देना ही आसन का कार्य है। दिन-प्रतिदिन जिज्ञासु स्वयं को निश्चल बनाने का प्रयत्न करता है। इससे रजोगुण (जिसका धर्म अस्थिरता है) संयम में रहता है। रजस् के संयत होने पर तमस् भी संयत हो जाता है; क्योंकि रजस् में ही तमस् विद्यमान रहता है। उच्च पदार्थ में निम्न भी समाया रहता है। इससे अन्तर्मन का तम-रूपी प्रमाद हट कर रज-रूपी चंचलता स्थिर हो जाती है; क्योंकि इसके अस्थिर होने पर मन भी अस्थिर हो जाता है, परन्तु संयमित होने पर शरीर का रोम-रोम सत्त्व के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है।
आसन निरन्तर अभ्यास से सिद्ध किया जा सकता है। आरम्भ में तो उचित आसन का पता लगाने में कठिनाई हो सकती है। किसी को पद्मासन लगाने में आसानी हो सकती है तो किसी दूसरे को सिद्धासन अथवा स्वस्तिकासन उपयुक्त प्रतीत हो सकता है। सबके लिए एक ही प्रकार का आसन अनुकूल नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार यह देख लेना चाहिए कि कौन-सा आसन उसके लिए उचित है। शरीर को भुलाये बिना मन को किसी एक लक्ष्य पर एकाग्र नहीं किया जा सकता।
तीन घण्टे तक एक ही आसन में बैठना आसन-जय कहलाता है। इससे शरीर पूर्णरूपेण सात्त्विक हो जाता है। रजस् एवं तमस् नष्ट हो जाते हैं। आसन-जय से व्यक्ति प्राणायाम की ओर अग्रसर हो सकता है। प्रारम्भ में यदि किसी आसन में बैठने से कष्ट हो तो आसन छोड़ कर थोड़ा विश्राम करना अत्यावश्यक है। थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक पथ में तो कुछ कष्ट सहन करना ही पड़ता है, इसके पश्चात् ही परमानन्द की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति हेतु अपना जितना भी उत्सर्ग करें, कम है। सच्चा साधक तो सदा यही सोचता है कि उसने अभी किंचित् भी त्याग नहीं किया। यह जानते हुए कि यदि आप अपनी जेब के अप्रचलित (खोटे) सिक्के फेंक दें तो आपका मित्र उसे स्वर्ण से भर देगा, आप सिक्के फेंक देते हैं तो इसे आप त्याग नहीं कह सकते। इसी प्रकार शाश्वत आनन्द की प्राप्ति हेतु इहलौकिक निस्सार पदार्थों का त्याग करना पड़ता है। अतएव तितिक्षा आवश्यक है। वेदान्त के अनुसार यह षट्सम्पत् अथवा छह गुणों में से एक है।
स्थिर आसन में बैठने का अभ्यास करने पर साधक को सात्त्विकता प्राप्त होती है। सत्त्वगुण-प्रधान होने पर प्राण सम हो जाते हैं और योगी श्वास को संयत करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करने लगता है।
आसन भी एक प्रकार की तपश्चर्या है। शरीर में सर्वदा चंचलता की प्रवृत्ति है। आसन द्वारा इस प्रवृत्ति को दूर किया जा सकता है। इससे आत्म-संयम प्राप्त होता है।
मुख्य आसन चार हैं- पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन एवं सुखासन। और भी आठ आसन हैं जिनमें दीर्घ काल तक सुखपूर्वक बैठना सम्भव हो सकता है।
आसन से शक्ति संचित रहती है। हिलने-डुलने से शक्ति का क्षय होता है। शरीर के क्रियाशील रहने पर अपेक्षाकृत अधिक प्राण-क्षय होता है, जब कि सर्वथा स्थिर आसन से उतने काल के लिए तो शक्ति के क्षय में कमी हो जाती है। शीत-प्रधान देशों में कुछ जीवों पर हैमन्तिकी प्रभाव देख कर आप इसे समझ सकते हैं। वे छह मास तक कोई भोजन नहीं करते; परन्तु उनकी शक्ति का नाश नहीं होता, क्योंकि वे चलना-फिरना आदि छोड़ देते हैं और इस प्रकार शक्ति संचित रहती है। शारीरिक शक्ति का यह संचय प्राणायाम द्वारा सूक्ष्म शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है और जिसे ध्यान में उपयोग किया जा सकता है।
स्मरण रखने योग्य एक और बात यह भी है कि आप आसनों का जितना ही अधिक अभ्यास करेंगे, उतनी ही अधिक नितान्त स्थिर मुद्रा में रहने की क्षमता आपको प्राप्त होगी। शारीरिक संवेदन कम होने लगेगा। आपका शरीर से सम्बन्ध सूक्ष्मतर होने लगेगा।
कायिक चेतना अति-स्थूल होने के कारण साधारणतया प्रत्येक क्रिया (संवेदना) का अनुभव बुद्धि ग्रहण करती है। यह अनुभव तीव्र स्नायविक कम्पन के रूप में होता है। आसन द्वारा स्नायविक ज्ञान की इस अवस्था में परिवर्तन आता है, शनैः-शनैः संवेदना की भावना नष्ट हो जाती है और संवेदना-जनित स्नायु-कम्पन कम होने लगता है। अतएव आसनों में सिद्धि प्राप्त करने पर आप धीरे-धीरे कायिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, प्रत्युत् यह एक प्रकार से शारीरिक तत्त्व का अतिक्रमण है। तब क्या होता है? शीत और उष्णता जैसे द्वन्द्वों का प्रभाव नहीं होता। शीतकाल में भी आप गंगा के किनारे बिना वस्त्र पहने बैठ सकते हैं। आपको सर्दी नहीं लगेगी। आसन-जय की यही अद्भुत शक्ति है। गंगा में बैठ कर यदि आप ध्यान भी लगायें और आसन स्थिर रखें तो आप अस्थिरता अथवा स्फुरण का अनुभव नहीं करेंगे। उच्चावस्थाओं में पहुँचने के लिए एक आसन में स्थिरता आवश्यक है; क्योंकि जब तक शरीर पर द्वन्द्वों का प्रभाव होता रहेगा, पन शरीर की ओर खिंचा आयेगा और अपने आन्तरिक लक्ष्य पर स्थिर नहीं रह सकेगा। आप जैसे-जैसे उन्नति करते हैं और आसन में अधिक-से-अधिक स्थिरता प्राप्त करते हैं, वैसे-वैसे द्वन्द्वों के अनुभव से आप ऊपर उठने लगते हैं। सर्वशक्तिमान् प्रभु का ध्यान करने से आसन में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। केवल इच्छा-शक्ति से ही शरीर में स्थिरता नहीं आ सकती।
शरीर स्थिर करने का रहस्य है मन को देह से दूर ले जायें। निराकार, सर्वव्यापक प्रभु के ध्यान में मन को एकाग्र करें। आकार का विचार ही मन से लुप्त हो जाना चाहिए। शरीर के प्रति विचार स्वतः ही लुप्त हो जायेगा। निराकार, असीम शक्ति का विचार करने से अभ्यासकर्ता सीमित शरीर को स्वयं ही भूल जाता है। इसे प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। निःसीम, निराकार का बोध होने पर परिमित आकार का ज्ञान नहीं रहता। परिणामतः शरीर उसी मुद्रा में रहने का आदी हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर काष्ठ अथवा शिला-खण्ड की भाँति हो गया है। आसन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का यही तो रहस्य है। मन को सीमित शरीर-तत्त्व से दूर रख कर अपरिमेय, अरूप, अनन्त का ध्यान करना आवश्यक है।
कतिपय भाष्यकारों का कहना है कि 'अनन्त' शब्द शेषनाग के अर्थ में लिया गया है, जिसने धरती को अपने फणों पर उठाया हुआ है; क्योंकि भार वहन करने पर हिलना कठिन होता है। कुछ अन्य भाष्यकारों के अनुसार अनन्त का अर्थ अपरिमेय है। स्थिर मुद्रा के द्वारा शरीर में पोषक तत्त्वों द्वारा परिवर्तन का क्रम न्यून होने लगता है। शरीर के स्थैर्य का मन एवं प्राण पर बहुत प्रभाव पड़ता है और शक्ति का हास नहीं होता। इस शक्ति को ध्यान में लगाया जा सकता है जिससे शरीर पर द्वन्द्वों का प्रभाव नहीं पड़ सकता।
प्राणायाम
प्राणायाम राजयोग का चतुर्थ अंग है। महर्षि पतंजलि अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से स्थूल कोश से सूक्ष्मतर कोशों की ओर अग्रसर होते हैं। प्राण और मन प्रगाढ़ रूप से परस्पर निबन्धित एवं एक-दूसरे से व्याप्त हैं। प्राणायाम का अर्थ है श्वास-प्रश्वास की गति को रोकना। शरीर के अन्दर सूक्ष्म एवं प्राणभूत शक्ति का स्थूल प्रतिनिधि श्वास ही है। घड़ी की चाबी पकड़ने से जिस प्रकार उसकी सूक्ष्म चरखियाँ घूमनी बन्द हो जाती हैं और अन्त में गोल स्प्रिंग भी रुक जाता है, उसी प्रकार मन को क्रियाशील करने वाली शक्ति को संयत करने से मन निष्क्रिय हो जाता है। यह प्राण-शक्ति ही है जो मन को चलायमान करती है। प्राण न रहे तो मानसिक क्रियाएँ भी नष्ट हो जाती हैं और मनोनाश जैसी अवस्था आ जाती है। प्राणों को निरुद्ध करना प्राणायाम है। जैसा कि हठयोग की पुस्तकों में दिया गया है, प्राणायाम नौ या दस प्रकार के नहीं हैं। हठयोग के शीतली, शीतकारी आदि विभिन्न प्राणायामों का यहाँ बताये गये प्राणायाम से सम्बन्ध नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल कुम्भक से है। एक बाह्य कुम्भक होता है। निःश्वास छोड़ कर पुनः अन्दर न लेना बाह्य कुम्भक है एवं श्वास अन्दर ले जा कर रोकना (फिर बाहर न लाना) आन्तरिक कुम्भक है। कभी-कभी श्वास स्वतः ही रुक जाता है। श्वास अन्दर हो अथवा बाहर, इसे केवल कुम्भक कहते हैं। प्राणायाम से मनुष्य के सभी अन्तरंग शुद्ध होते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि मनुष्य में सत्त्व, रजस् और तमस् तीनों प्रकार के गुण विद्यमान हैं। अपने समक्ष लक्ष्य यह ही होना चाहिए कि अधिक-से-अधिक मात्रा में सत्त्वगुण की अभिव्यक्ति और स्फुरणा हो; किन्तु अशुद्धता का परदा सत्त्वगुण को पूर्ण रूप से स्फुटित नहीं होने देता। प्राणायाम इस परदे को हटा कर सत्त्वगुण को आभासित करता है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य यही है। मन एवं प्राण एक-दूसरे से अविच्छिन्न रूप से सम्बन्धित हैं, अतः मन को निष्क्रिय करके इसे शुद्ध करना चाहिए एवं तदुपरान्त सत्त्वगुण की अभिव्यक्ति में बाधक आवरण को दूर करना चाहिए। सत्त्वगुण-प्रधान होने पर सुविचार के लिए मन में स्थान रह जाता है और मनुष्य यम-नियम के पालन में दृढ़ हो जाता है। सब ठीक होने लगता है। मन स्थिर हो जाता है और ध्यानाभ्यास हेतु दक्षता प्राप्त हो जाती है। प्राणायाम का उद्देश्य है-साधक को ध्यानाभ्यास के योग्य बनाना।
प्रत्याहार
अष्टांगयोग के पूर्व-कथित चतुष्टांग योग की भूमिका मात्र हैं, वास्तविक योग नहीं। ज्ञानयोग में योग का अर्थ निदिध्यासन लिया गया है। ध्यानरत होने के लिए सद्गुरु से निरन्तर उपनिषदों के प्रवचन सुनने की आवश्यकता है। विचार यदि निरन्तर इसी प्रकार के बने रहें तो फल-प्राप्ति अवश्य होती है। प्रतिदिन गुरु आपको यही तो सिखाते हैं : 'आप यह शरीर नहीं, यह चंचल मन नहीं, अपितु अविनाशी नित्य आत्म-स्वरूप हैं।' यही सुन कर आत्म-चैतन्यता जागृत होती है। प्रत्यक्ष प्रेरणादायक एवं सात्त्विक विचार जो आपके नित्य स्वभाव को प्रकट करते हैं, इस सुप्त आत्म-तत्त्व के स्वाभाविक अंग हैं। सुप्त आत्म-तत्त्व में, इन सुविचारों का जब अविरत प्रवाह होता है तो अशुद्ध विचारों का स्थूल आवरण धीरे-धीरे विच्छिन्न होने लगता है और सात्त्विक अथवा आध्यात्मिक विचार ही चेतना के केन्द्र में प्रवेश करते हैं। तब आप स्वयं में एक विशेष परिवर्तन का अनुभव करते हैं। ऐसे भाव कि 'मैं यह शरीर हूँ', 'मैं दुःखी हूँ' आदि धीरे-धीरे तिरोहित होने लगते हैं और आप इस शरीर से बन्धन-मुक्त-सा अनुभव करने लगते हैं। आपके चेतन तत्त्व में सूक्ष्म परिवर्तन आने लगता है। शरीर में होने वाले अनुभवों hat H आप अप्रभावित रहने लगते हैं। इस प्रकार का एक अदृश्य परिवर्तन होता जाता है।
तत्त्वज्ञानी कहते हैं : 'आप सच्चिदानन्द हैं, आप नित्य हैं, शाश्वत हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। आपको कोई रोग नहीं, कोई कमजोरी नहीं और आपमें कोई अपूर्णता नहीं। आप सदा सम्पूर्ण दिव्य आत्म-तत्त्व हैं। इस तथ्य को भूलने पर ही आप सोचते हैं कि आप केवल यह शरीर मात्र हैं।'
युवावस्था में पहुँच कर भी आप उसी 'मैं' का प्रयोग करते हैं जिसका आप बचपन में अपने प्रति किया करते थे। आपकी संस्थिति भिन्न हो गयी है, भावों में परिवर्तन आ गया है और लक्ष्य भी कुछ और हो गया है, तथापि इस 'मैं' भाव में अन्तर नहीं आया। यद्यपि आप परिवर्तित अनुभव करते हैं, यथापि 'अहं' वही है। पिता बनने के पश्चात् आप कई उत्तरदायित्व भी सँभालते हैं; परन्तु आपका 'अहं' अच्छी प्रकार जानता है कि आप वही हैं जो कभी बच्चे थे, फिर यौवन में प्रवेश किया और समय आने पर विवाह किया। बाबा (पितामह) बनने पर भी आप यही जानते हैं और अनुभव करते हैं कि 'मैं' बालक था, किशोर था, वयस्क हो कर विवाहित हुआ और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। 'मैं' वही है। यही मैं या अहं सच्चिदानन्द है। 'मैं यह काया नहीं हूँ,' मन में यह भाव रखने से आपको स्थूल चेतन तत्त्व व्याकुल नहीं कर सकता। बाद में बाह्य शरीर की स्थूल क्रियाएँ भी आप पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकतीं। स्थितप्रज्ञ की अवस्था का वर्णन भगवद्गीता में है। श्रवण एवं मनन करना चाहिए। इसके पश्चात् ध्यानावस्था प्राप्त होती है जिसमें सब विक्षिप्त विचारों का सर्वथा निराकरण हो जाता है और आन्तरिक एवं बाह्य प्रकृति की शुद्धि होती है।
अपने में धर्म-भाव के सद्गुणों का विकास करके कर्म की शुद्धि को, जिसके फल-स्वरूप आप पुण्यशील बन जायें और कुकर्म न करें, यम कहा जाता है। यम पालन के उपरान्त नियम आपकी दैनिक क्रियाओं को प्रभु की ओर उन्मुख कर देता है। आसनों द्वारा शरीर के अन्तरतम में स्थित भाग जो पाँच तत्त्वों से बने हैं और जिन्हें हम पंचकोश कहते हैं, में सम्पूर्ण सात्त्विक शक्ति का संचार किया जाता है। तदुपरान्त आप श्वास नियमित करके प्राणायाम द्वारा सूक्ष्म (प्राणिक कोश) की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्वास नियमित करके मत संयत किया जाता है और इसके उपरान्त प्राणायाम द्वारा सात्त्विक प्रकृति आभासित होती है।
सम्यक् योग पाँचवें अंग से आरम्भ होता है, जिसका मुख्य विषय 'मन' है। योग की सर्वोच्च उपलब्धि में सहायक मन ही है। अपवित्र मन योग में सदा बाधा-स्वरूप है; परन्तु मल-रहित पवित्र मन संयम में रहने से योग का निमित्त बन जाता है। इतने पर भी यह स्मरणीय है कि मन की सहायता एक सीमा तक ही अपेक्षित है। इसके उपरान्त वह भी बाधक हो जाता है।
योग का उद्देश्य मन का अतिक्रमण है। उदाहरण के लिए एक बड़ी-सी पतंग को ही लीजिए। उसे उड़ाने के लिए इसमें धागे को जोड़ने की आवश्यकता होती है, स्वतः ही इसका उड़ना असम्भव है। धीरे-धीरे धागा खींच कर इसे ऊपर उड़ाया जाता है; परन्तु अन्तरिक्ष में पहुँचने पर धागा बाधा बन कर रह जाता है। उस समय पतंग धागा तोड़ कर अन्तरिक्ष में और ऊपर जाने लगती है। मन की भी यही दशा है। प्रथमावस्था में तो उन्नति के हेतु मन की सहायता आवश्यक है; परन्तु अन्ततः मन से भी परे जाना है। किसी ऊँची छत पर आरोहणार्थ सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है; परन्तु सीढ़ी के अन्तिम सोपान पर पहुँचते ही इसे त्याग दिया जाता है। साधना की एक विशेष अवस्था प्राप्त हो जाने पर योगी को ज्ञात होता है कि मन उसके अभ्यास में बाधक बन रहा है। यह अनन्त पदार्थों की ओर भटकता रहता है। अनेक पदार्थों में इसकी आसक्ति है और निरन्तर उनका सेवन करने से अथवा उनके संग रहने से एक प्रकार की मनोपरायणता उत्पन्न हो जाती है। पदार्थों के होने पर तो उनके प्रति आसक्ति का ज्ञान नहीं होता; परन्तु जब वे पदार्थ पास नहीं होते तो उनके अभाव की अनुभूति होती है। अतएव, योगी का प्रथम कर्तव्य है बाह्य तत्त्वों की ओर से मन को समेटना। आप बाहर किसे ढूँढ़ रहे हैं? असीम आनन्द तो आपके अन्तर्मन में ही सन्निहित है। बाह्य तत्त्व आपका लक्ष्य नहीं है।
लक्ष्य-प्राप्ति के हेतु आप कोई भी मार्ग अपना सकते हैं; परन्तु मन की बाह्य पदार्थ की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है। कभी तो मन से अनुनय करना पड़ सकता है और कभी इसे आत्म-शक्ति द्वारा वश में करना आवश्यक हो जाता है। मन को वशीभूत करने के लिए प्राणायाम भी सहायक हो सकता है। तात्पर्य यह है कि अन्यान्य विधि से इनकी विषयोन्मुखता को दूर करना है। इसी पाँचवी अवस्था में योगी को इस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए कि मन इन्द्रिय-विषय से विरक्त हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु सब इन्द्रियों को वश में करना आवश्यक है। इसके उपरान्त अपेक्षित है एकान्तवास।
योगी को एकान्तवास क्यों प्रिय होता है? क्योंकि एकान्त-स्थान में आकर्षित करने वाले चक्षु-विषय नहीं होते। एकान्तवास द्वारा इन्द्रियों की विषयासक्ति का प्रभाव एकबारगी ही कम हो जाता है। अतः प्रत्याहारार्थ योगी को शहरों में अथवा जन-संकुल बस्तियों में नहीं रहना चाहिए। मन को निरन्तर विषयोन्मुख नहीं रखना चाहिए। बाद में तो सावधानीपूर्वक सर्वत्र भ्रमण की आज्ञा है; परन्तु प्रत्याहार के अभ्यास के आरम्भ काल में यह आवश्यक है कि योगी एकान्तवास करे जिससे कि मन का बाह्य विषयों से विमुखीकरण सुसाध्य हो सके। पौधा लगाने पर उसकी रक्षा अनिवार्य है, अन्यथा एक मेष-वत्स भी इसे खा सकता है। इसी प्रकार प्रारम्भिक अवस्था में योग का रक्षण एकान्तवास द्वारा अनिवार्य है। पौधा जब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, तब उसकी रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उस समय तो हाथी को भी उसके साथ बाँध दिया जा सकता है।
आपके मन में प्रश्न उठ सकता है- 'शिवानन्दाश्रम के आनन्द कुटीर में इतना जन-समूह क्यों आता रहता है?' यहाँ हमने शिष्यत्व का पथ चुना है। और स्थानों से यह स्थान कुछ अलग-सा है। यहाँ गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी का अपार कृपा-वेग सदा प्रभामण्डल में निवास करता है। अतएव, समस्त योग यहीं केन्द्रित तथा यहीं से वर्गीकृत होते हैं। यह स्थान एक दुर्ग समान है। ब्रह्मज्ञानी तपस्वी की अपार कृपा की सन्निधि (समुपस्थिति) ही हमारे लिए दुर्ग-रूप है। यहाँ योग गुरु-कृपा से रक्षित रहता है; क्योंकि आत्मा गुरुदेव के कार्यों में निरत रहती है। आपको यहाँ इतस्ततः आने-जाने की आज्ञा नहीं होती। मन इधर-उधर नहीं भटकता। इसीलिए प्रत्याहार की अवस्था में संरक्षण की आवश्यकता होती है। दिनोंदिन प्रत्याहार का अभ्यास करने के उपरान्त मन को अन्तर्मुखी होने का अभ्यास हो जाता है। तत्पश्चात्, विषयों से सम्पर्क स्थापित होने पर भी इन्द्रियाँ संयत रहती हैं, आकृष्ट नहीं होतीं; क्योंकि मन अन्तर्मुख होने लगता है।
यदि मन इन्द्रिय-विषयों से जुड़ा रहता है तो इन्द्रियाँ भी विषयासक्त हो जाती हैं। यदि मन आपके आदर्श में ही निविष्ट हो तो वह सदा सुकार्यरत रहता है और इन्द्रियाँ मोह-माया से आकर्षित नहीं होतीं। असावधानी के क्षणों में ही इन्द्रियाँ माया-जाल में फँस सकती हैं; परन्तु साधारणतया इन्द्रियाँ अन्यान्य विषयों से उत्तेजित नहीं होतीं। ऐसी अवस्था में विषयों का समापतन होने पर भी इन्द्रियाँ मन को प्रभावित नहीं करतीं। अतः प्रत्याहार की अवस्था में यदि आप ऋषिकेश के बाजार में जायें और रेडियो पर कोई भावुक संगीत सुनें, तब भी आपके मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप केवल आवाज ही सुन पायेंगे; क्योंकि आपके मन की एक पृष्ठभूमि है, अतः मन गाना सुनते हुए भी नहीं सुनेगा।
यह आवश्यक नहीं कि यदि आप किसी पदार्थ को देख रहे हैं तो आप वास्तव में ही उसका अवलोकन कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं; पर हो सकता है अवधारण नहीं कर रहे हैं। स्पर्श कर रहे हैं, पर अनुभव नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार मन का इन्द्रियों से सम्बन्ध धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। मन को उचित भूमिका प्राप्त होने पर यह अन्तर्वर्ती होने लगता है; परन्तु वह भूमिका है आपका आदर्श। इसके अनेक रूप हैं। यह आदर्श एक विचार-श्रृंखला भी हो सकता है, जीवन का एक विशेष सुसंस्कृत रूप हो सकता है जिसमें आप स्वयं को ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोई महापुरुष हो सकता है जिसके आदर्शों का आप अनुसरण करना चाहते हैं। इस प्रकार मन को जिस प्रकार की पृष्ठभूमि प्राप्त है, उसी द्वारा वह अन्तर्वर्ती हो जाता है एवं इन्द्रियाँ भी विषयों के प्रति आकर्षित होने का अपना स्वभाव त्याग देती हैं। मन के इस प्रकार सिमटने पर ही वह आगामी ध्यान-भूमिका, धारणा (एकाग्रता) के लिए तैयार होता है। मन को एकाग्र करने से पूर्व इसे सब ओर से हटा कर समेटना आवश्यक है। मन को एक लक्ष्य पर एकाग्रित करने की इस प्रारम्भिक प्रक्रिया के क्रम को प्रत्याहार कहते हैं। इसमें मन की रश्मियाँ एकत्र करके केन्द्रित की जाती हैं। राजयोग के षष्टांग में बाह्यता से हटे हुए मन को ध्यान-लक्ष्य पर केन्द्रित करना बताया गया है। इसे धारणा अर्थात् ध्यान-बिन्दु पर मन को दृढ़तापूर्वक एकाग्र करना कहते हैं। यही वास्तविक योग है। योग का अर्थ है अनन्यमनस्क ध्यान, जिसके द्वारा आत्म-साक्षात्कार की ज्योत्स्ना प्राप्त होती है। ध्यान के समय कौन-कौन-सी बाधाएँ समक्ष आती हैं एवं एकाग्रता के समय मन किस प्रकार कार्य करता है, इन सबकी विवेचना आगामी पृष्ठों में की जायेगी।
धारणा
धारणा एकाग्रता का अभ्यास
एकाग्रता सतत रूप में संलग्नतापूर्वक प्रयत्न करने का विषय है। एक ही दिन में इसके अभ्यास की फल-प्राप्ति असम्भव है। यह ऐसा कर्म नहीं जो अकस्मात् ही रात-भर में ही अपना प्रभाव दरसा दे। प्रत्युत्, आरम्भ में तो यह प्रक्रम अतीव अरुचिकर एवं दुःखदायी है; क्योंकि मानव-मन स्वभाव से ही अस्थिर है, अनेक पदार्थों में भटकता रहता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर भागना इसका गुण है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह टिड्डे के समान है जो सदा स्फुरणशील रहता है। यह बहिर्मुखी है। यदि आप मन की प्रकृति को परिवर्तित करके इसे बाँधने अथवा एक ही लक्ष्य पर एकाग्र करने का प्रयत्न करेंगे तो स्वाभाविक ही है कि यह विकट बन्धन का अनुभव करेगा एवं उससे मुक्त होना चाहेगा। अतः साधक को दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। भव्य ध्येय को ध्यान में रखते हुए उसे सर्वदा संघर्ष करते रहना चाहिए; क्योंकि अन्ततः यह प्रयत्न ही उसे असीम आनन्द की ओर ले जायेगा।
साक्षात्कार की चरम शक्ति के प्रति पूर्ण प्रतीति एवं दृढ़ विश्वास प्राप्त करने के उपरान्त ही साधक ध्यान के कठिन और शुष्क क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा, ध्यानावस्था में पहुँचने पर भी साधक को किसी प्रकार की ज्योति नहीं मिलती। कई दिवस, माह एवं वर्षों पर्यन्त अभ्यास करने पर भी उन्हें कोई सफलता दृष्टिगोचर नहीं होती और वे निराश हो जाते हैं। इसीलिए तो अनुभवी एवं तत्त्वज्ञानी की छत्रछाया में साधना-विधि सीखने का आदेश दिया गया है। वे साधकों को अनेक युक्तियाँ बताते हैं, जिससे वे ध्यान में रुचि ले सकें। मन के ऊब जाने पर वे उसे मार्ग पर लाने के लिए अन्यान्य उपाय निर्दिष्ट करते हैं।
ध्यान के लिए आपका जो भी निर्दिष्ट लक्ष्य अथवा केन्द्र है, आप यदि उस पर ध्यान करते थक गये हैं, आपका मन नहीं लग रहा, तो ठीक है, छोड़ दीजिए एवं उस क्षण-विशेष में उस वस्तु का ध्यान कीजिए जो आपको बहुत प्रिय हो। उस पदार्थ पर अपना ध्यान केन्द्रित करने का यत्न करें जो मन को अतीव रुचिकर हो और जिस पर मन अविरत गति से अधिक समय तक एकाग्रित रह सके। इस प्रकार मन निविष्ट हो जायेगा। यह त्तो मानसिक शिक्षण का विषय है। ध्यान की प्रक्रिया को यथा-सम्भव सुखद और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आपको अनेक उपायों को अपनाना पड़ता है। किसी समय यदि ध्यान न लगे तो पुस्तकों का अध्ययन अथवा कीर्तन करना आरम्भ कर देना चाहिए। चित्तवृत्ति का पुनः रुझान होने पर पुनः ध्यान में बैठ जाना चाहिए।
ध्यान को सुखकारी एवं सुरुचिकर बनाने के लिए सदा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप स्वयं को भाव से भरिए। भक्त ही भाव का लाभ प्राप्त कर सकता है, राजयोगी नहीं। भक्त के लिए ध्यान सदा सुखावह होता है; क्योंकि उसे अपने प्रियतम का चिन्तन अच्छा लगता है। परन्तु वेदान्ती को प्रेरणा-तरंगों का आह्वान करना पड़ता है जैसे 'मैं आनन्दमय हूँ, अवर्णनीय आनन्द हूँ' आदि। वह इस प्रकार के उत्कर्ष से पूर्ण होने का यत्न करता है।
इतना होते हुए भी मन को वशीभूत करना सुगम नहीं है। किसी विशेष ध्वनि पर ध्यान केन्द्रित करना, प्रणव का जप करना अथवा मन्त्र-विशेष पर ध्यान लगाने का यत्न करना आदि विभिन्न उपाय हैं जिनसे मन निरन्तर कार्यरत रहे और उसे इतस्ततः भागने का समय ही न मिले। इतना करने पर भी कभी-कभी ध्यान लगाना कठिन-सा प्रतीत होने लगता है। आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि ध्यान कब रोकना है। यह नहीं कि यदि मन नहीं चाहता तो ध्यान लगाना छोड़ दिया जाये। बुद्धिमत्ता एवं चतुरतापूर्वक आपको मन की क्षमता का पता लगाना चाहिए एवं कभी-कभी नियमित रूप से उसकी इस क्षमता को जाँच लेना चाहिए। कभी-कभी जब ऐसा प्रतीत हो कि मन आपको अकारण ही मार्गच्युत कर रहा है तो आपको चाहिए कि अपनी शक्ति द्वारा उसे संयम में रखने का प्रयत्न करें और ध्यान में लगायें; परन्तु यदि फिर भी ऐसा लगे कि मन आपके वश से बाहर है और आप उसे वश में करने में अशक्त हैं, तो कोई अन्य उपाय काम में लाना चाहिए। मन का इस प्रकार अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। प्रत्येक बार आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि मन शान्त है अथवा अशान्त। बुद्धिमत्ता एवं विवेकशीलता से ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ध्यानाभ्यास के बारम्बार करने पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए अतिरिक्त, ध्यान को स्थिर और सफल बनाने के लिए किंचित् अप्रत्यक्ष साधन भी हैं।
यह साधन कौन-कौन-से हैं, इसका वर्णन आगे किया जायेगा।
वैराग्य
साधारणतया आपको यह शिकायत रहती है कि जब आप ध्यान लगाने का यत्न करते हैं तो मन इधर-उधर भागता है। आप मन को एकाग्र नहीं कर सकते। आपको स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि 'मन इतस्ततः क्यों भटकता है?' 'यह कहाँ जाता है?' इसका पता लगाना अत्यन्त कठिन है। अर्धचेतन मन में ही कुछ अशान्ति होती है। यदि आप पूछें, 'क्यों और कहाँ अशान्ति होती है?' तो इसका उत्तर है कि कुछ विचार आ कर मन को व्याकुल करते हैं और ये विचार किसी व्यक्ति के, किसी अनुभव के अथवा पूर्व-स्मृति के सम्बन्ध में होते हैं। विचार सदा किसी-न-किसी बाह्य जगत्, बाह्य अनुभवों से सम्बन्धित होते हैं। आत्म-परीक्षण करने पर आपको प्रतीत होगा कि मन उन पदार्थों की ओर भागना चाहता है जिनमें उसकी आसक्ति एवं रुचि है। यह इच्छा या रुचि अर्धचेतन मन में छिपी होती है जिसका सम्भवतः आपको ज्ञान भी नहीं होता।
आसक्ति इच्छा जैसी ही है। आसक्ति एवं इच्छा का अटूट साथ है। जहाँ आसक्ति होगी, वहाँ पदार्थ के प्रति इच्छा भी होगी। अतएव, अन्तिम परीक्षण इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि आसक्ति और इच्छा ध्यान में विघ्न-स्वरूप हैं। इन्हें राग-द्वेष भी कहते हैं। आप या तो उस पदार्थ का चिन्तन करते हैं, जो आपको प्रिय नहीं अथवा उसका चिन्तन करते हैं जो आपको प्रिय है और जिसमें आप आसक्त हैं। अतः समस्या का मूल केवल आसक्ति एवं अविरक्ति है। इसका अर्थ है वैराग्य की कमी।
यदि आपमें वैराग्य-भाव नहीं तो मन अन्यान्य विषयों में आसक्त होता ही रहेगा। आपको प्रतीत होना चाहिए कि वैराग्य का अभाव एकाग्रता का शत्रु है। भगवान् कृष्ण अर्जुन से कहते हैं: 'मन का निग्रह अतीव दुष्कर है, इसमें सन्देह नहीं कि यह कार्य कठिन है, परन्तु निरन्तर अभ्यास से एवं वैराग्य की सुदृढ़ता से यह सम्भव हो सकता है।' वैराग्ययुक्त बनना चाहिए। इच्छाओं एवं मोह-माया का त्याग कर देना चाहिए। वैराग्य योग-साधना का रक्षक एवं अनिवार्य अंग है। अविरत उद्यम द्वारा आप पूर्ण वैराग्य की अवस्था में अधिष्ठित होने का प्रयत्न कर सकते हैं जो विवेक द्वारा ही प्राप्त होती है।
दिन के चौबीस घण्टे ही आपको प्रबुद्ध रहना चाहिए। विवेक-बुद्धि को चलते ही रहना चाहिए। विवेकशील व्यक्ति ही किसी पदार्थ के बास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जहाँ विवेक नहीं होगा, इच्छा उत्पन्न हो जाती है और मन इतस्ततः भागता है। परिणामतः ध्यान में एकाग्रता नहीं आती। तृष्णा एवं वैराग्य का अभाव ही विक्षेप का मूल कारण है। राजयोग के छठे अंग 'ध्यान' की अवस्था तक पहुँचने पर हमें सर्वदा स्मरण रखना है कि अभ्यास और वैराग्य ध्यान के निर्देशक तत्त्व हैं। ध्यान में सफलता पाने के अभिलाषी योगी को यह युग्म सदा स्मरण रख कर जीवन में इनका अभ्यास करना चाहिए।
ध्यान में और किससे सहायता मिलती है? एकाग्रता का सम्बन्ध प्रमुखतः मन से है, परन्तु हम जानते हैं कि मन का सम्बन्ध प्राण से है तथा प्राण इहलौकिक विषय-वासनाओं में आसक्त शरीर से जुड़ा है। इसलिए मानव के सम्पूर्ण क्रियाशील जीवन से मन सम्बन्धित है। इसके आधार पर हमें कुछ सिद्धान्त बनाने चाहिए जो ध्यान के सम्बन्ध में कतिपय सुझाव देते हुए हमारा मार्ग-निर्देश करें।
एकान्तवास एवं सात्त्विक भोजन
योग-मार्ग प्रवृत्त होने पर जहाँ तक सम्भव हो सके, सब बाह्य सम्बन्धों के त्याग करने का यत्न करना चाहिए। दैनिक जीवन में उन सब सम्बन्धों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए जो योग-मार्ग के विरुद्ध ले जाने वाले हो। उस स्थान पर, उस व्यक्ति के संग अथवा उस वातावरण में नहीं रहना चाहिए जो मन को बहिर्मुखी करता हो और उसमें तृष्णा जाग्रत करता हो। विषयासक्त करने वाले एवं वैराग्य में विघ्न लाने वाले सब पदार्थों का त्याग अनिवार्य है। यही कारण है कि ध्यानावस्था तक पहुँचने पर विद्वज्जनों के अनुसार योगी को समाचार-पत्र अथवा उपन्यास आदि नहीं पढ़ने चाहिए और न सांसारिक लोगों से सम्बन्ध ही रखना चाहिए। मोह का त्याग करना चाहिए। आध्यात्मिक वातावरण के स्थान में ही वास करना चाहिए। आस-पास का वातावरण प्राकृतिक एवं सुन्दर होना चाहिए। पुण्यात्माओं से सम्पर्क रख कर आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए। सच्चे साधकों एवं साधुजनों के साथ विचरण करना चाहिए।
संसार के माया-जाल में फँसे हुए लोगों के साथ आप सम्पर्क रखेंगे तो क्या होगा ? उनका सम्पर्क आन्तरिक जीवन को सर्वथा दूषित कर देगा। अतएव यदि आपमें एकाग्र होने और ध्यान करने की लगन है तो आपको अपना बाह्य जीवन भी जहाँ तक सम्भव हो सके, साधना-निष्ठ करना होगा। इसमें भोजन भी विशेष कारण है। राजसिक अथवा तामसिक भोजन करने से मन सन्तुलित नहीं रहेगा और साधना पर कुप्रभाव पड़ेगा। सबसे हानिकर आदत शराब पीने की है। कोई व्यक्ति यदि शराब भी पीता है और ध्यान में अधिष्ठित होना चाहता है तो क्या उसे सफलता मिल सकती है? कदापि नहीं। शराब का प्रभाव नैतिक पतन करने वाला होता है, जब कि योग का उद्देश्य है अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर संयम प्राप्त करना। शराब एवं संयत जीवन के मध्य अनेक ऐसे पदार्थ हैं जो मन पर शराब की भाँति प्रभाव नहीं डालते; परन्तु उनका संचित प्रभाव शराब के वेग से भी अधिक हानिकारक होता है। यदि निरन्तर असात्त्विक भोजन, जो एकाग्रता में सहायक नहीं है, करते रहें तो मन चंचल हो जायेगा, अशान्त रहने लगेगा। अतएव भोजन सात्त्विक ही लेना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है।
सत्त्वगुण युक्त भोजन योगाभ्यास के अनुकूल रहता है। दैनिक अभ्यास की दृष्टि से भी आपको देखना चाहिए कि भोजन ऐसा हो जो एकाग्रता लाने में विघ्न-रूप न बने। असन्तुलित भोजन एवं अति-आहार मुख्य कारण हैं जिनसे मन एकाग्र नहीं रह सकता। अति-आहार से शरीर का सारा रक्त उदर की ओर प्रवाहित होने लगता है। एकाग्र होने के लिए सारा रक्त मस्तिष्क की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। आसन में बैठने से अधिक-से-अधिक रक्त मस्तिष्क की ओर जाता है, परन्तु अति-आहार करने पर अधिकतर रक्त उदर की ओर जायेगा और ऐसी अवस्था में यदि आप रक्त-प्रवाह को मस्तिष्क की ओर ले जाना चाहेंगे तो उदर विरोध करेगा और परिणाम-स्वरूप अनन्यमनस्क होने की अपेक्षा तन्द्रिल होने लगेगा। तन्द्रा का अनुभव अति-आहार से ही होता है।
यदा-कदा ऐसा भी होता है कि भोजन तो आप सन्तुलित ही लेते हैं; परन्तु उसमें कुछ तत्त्व ऐसे होते हैं जो वायु उत्पन्न करते हैं। वायु होने से प्राण में विकार उत्पन्न हो जाता है और वह असन्तुलित हो जाता है। अतएव, साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। यदि वे ध्यान में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें आलू एवं कद्दू का त्याग करना चाहिए। यदि त्याग न कर सकें तो उनका प्रयोग कम करना चाहिए। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो सामान्यतः वायु-विकारक तो नहीं होते, परन्तु कुछ विशेष व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कहने को तो खाद्य-विशेष सात्त्विक हो सकता है; परन्तु सम्भव है आपकी प्रकृति के अनुकूल न हो। ऐसे पदार्थों का परित्याग कर देना चाहिए। आपके प्रतिदिन के अभ्यास एवं नियम में भोजन का तत्काल प्रभाव क्या पड़ता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
भोजन के सम्बन्ध में उपर्युक्त विचार शारीरिक दृष्टिकोण से किया गया है। भोज्य पदार्थों एवं बाह्य वातावरण के प्रति सावधान रहिए। मन को अन्तर्मुखी कीजिए। व्यावहारिक जीवन में साथियों के साथ विचरण करते समय प्रयत्न कीजिए कि दैनिक व्यवहार में आप पर कम-से-कम संस्कार पड़े। रात्रि की गहरी निद्रा के उपरान्त प्रातः-समय मन सर्वथा शान्त होता है। इसके पश्चात् सारा दिन आप कई प्रकार के लोगों के साथ घूमते या रहते हैं। कुछ लोगों से आप क्रोधित हो जायें तो आपका मन इस प्रकार के संस्कारों से क्षुब्ध हो सकता है। दिन का अन्त होने तक मन की दशा अति व्याकुल हो सकती है। प्रातः से सायं पर्यन्त जो-कुछ भी हुआ, उससे आप चिन्तित होने लगते हैं, परन्तु इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? व्यावहारिक जीवन में भी सब प्रकार से सन्तुलन रखने का यत्न करना चाहिए। केवल सच्ची लगन से अभ्यास करने पर ही शान्ति एवं क्षमता प्राप्त की जा सकती है। आपको कैसे भी अनुभव क्यों न हों, प्रत्येक स्थिति में अपने मन को सन्तुलित रखें।
प्रत्याहार का अभ्यास नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इससे बाह्य पदार्थों के सम्पर्क में आने पर भी वे मन पर अपना गहन प्रभाव नहीं छोड़ सकेंगे। यह अवस्था स्वतः प्रवर्तित अन्तर्मुखी होती है। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि अपने कार्यों की उपेक्षा की जाये। कुछ मनोवृत्ति तो कार्य करने के लिए जागृत रहनी चाहिए और शेष अधिक अन्तर्मुखी हो जानी चाहिए। बाह्य रूप से जागरूक रहना एवं साथ ही मन को अन्तर्वर्ती करने का यह क्रम ईश्वर के निरन्तर स्मरण में अतीव सहायक है। 'ॐ' अथवा किसी मन्त्र का जप करें, साथ ही अन्दर मन में कुछ विचार भी रखें; क्योंकि मन एक क्षण के लिए भी शून्य नहीं रहना चाहिए।
कुछ व्यक्तियों में मन की पृष्ठभूमि नहीं होती। उनके मन में भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं। एक कार्य सम्पन्न होने पर साधक के मानस-पटल पर तुरन्त अपने इष्ट की प्रतिमा आ जानी चाहिए। मन को इस क्रिया में अभ्यस्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार साधक के कार्यरत रहने पर भी मन अपनी पृष्ठभूमि पर स्थिर रहेगा और बाह्य जगत् उसे प्रभावित नहीं कर सकेगा। इस कला में निपुणता प्राप्त कर लेने पर आप किसी भी कार्य में लगे रहें, उससे प्रभावित नहीं होंगे। प्रत्याहार का ऐसा विकास कर लेने पर मन जीवन के प्रतिदिन के संस्कारों के बन्धन से मुक्त रहता है।
ध्यान अथवा एकाग्रता एक प्रतिशत अध्ययन और निनानवे प्रतिशत अभ्यास पर आधारित है। एकाग्रता के लिए किसी भी सीमा तक अध्ययन अथवा प्रवचन सुनना लाभकारक नहीं होता। इसमें केवल दैनिक अभ्यास द्वारा ही सफलता प्राप्त हो सकती है और यदि कोई कठिनाई भी आये तो वह भी अभ्यास द्वारा सुलझ जाती है। यदि आप सोचें कि पहले मार्ग में आने बाली समस्याओं का हल ढूँढ़ लिया जाये और फिर ध्यान लगाया जाये तो आप ध्यान कभी नहीं लगा सकेंगे। केवल अभ्यास ही ध्यान में सफलता की कुंजी है।
एकाग्रता के विविध रूप
मन की एकाग्रता ही वास्तविक रूप में योग का दर्शन कराती है। हमने देखा है कि किसी धर्म अथवा जाति में, अन्तिम लक्ष्य पर पहुँचने का साधन गहन ध्यान का अभ्यास ही है। कोई भी धर्म हो, आध्यात्मिक जीवन के बाह्य आचरण भी चाहे कैसे ही हों, साधक को अपनी मंजिल पर पहुँचने का मुख्य मार्ग ध्यान ही बताते हैं। यह क्रम राग एवं वैराग्य का है, अर्थात् स्वयं को नाम और रूप के इस भौतिक जगत् से अलग करके अन्तरस्थ सत्य, परम सत्य से सम्पृक्त करना। दूसरे अर्थ में इन्द्रियों को बाह्य जगत् के प्रवृत्तिजन्य ज्ञान hat H दूर करके आत्म-तत्त्व को गन्तव्य लक्ष्य का बोध कराना। योगाभ्यास का मुख्य क्रम यही है। सब आध्यात्मिक क्रियाएँ इसी क्रम पर आधारित हैं। संसार से परे के क्षेत्रों की ओर जाने का मुख्य द्वार यही है। अतएव, ध्यान लगाने की कला साधक द्वारा सद्गुरु के चरणारबिन्द में बैठ कर ही सीखी जा सकती है; क्योंकि आध्यात्मिक क्रिया होने के नाते यह एकाग्रता की उस कला से सर्वथा भिन्न है जो जीवन के अन्य क्षेत्रों के कार्यों में लक्षित होती है। एकाग्रता सर्वत्र अनिवार्य है। एकाग्रता के बिना किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता सम्भव नहीं है। एक वैज्ञानिक अपने अनुसन्धान-कार्य में मन को एकाग्र करता है तो कलाकार का मन अपनी प्रतिमा में केन्द्रित रहता है, जो उसे चित्रित करनी है। संगीतज्ञ अपने संगीत में खोया रहता है तो घड़ीसाज़ अपने कार्य में अनन्यमनस्क रहता है। किन्तु इस प्रकार की एकाग्रता केवल मानसिक स्तर तक ही सीमित है; अतएव बाह्य है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह एकाग्रता सर्वथा भिन्न है। यहाँ तक कि तान्त्रिक अथवा गुह्य विद्या के ज्ञाता की एकाग्रता भी जो अप्रत्यक्ष दर्शन की क्षमता का विकास करना चाहता है, स्थूल प्रकार की ही होती है; क्योंकि यह उसके अहं-बोध पर आधारित है। वे अपने स्थूल कायिक बोध से ऊपर नहीं उठ सके हैं। सम्मोहित करने की क्षमता विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार की एकाग्रता का अभ्यास आवश्यक होता है; परन्तु उसमें आध्यात्मिक आदर्श नाम मात्र भी नहीं होता। इसीलिए एकाग्र होते समय भी उसका ध्यान मायावी व्यक्तित्व पर ही आधारित होता है।
स्वतः व्यक्तित्व को अस्वीकारते हुए दृढ़प्रतिज्ञ हो कर यह विचारना चाहिए कि 'मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इस नश्वर संसार से सम्बन्धित नहीं हूँ, मैं सदा मुक्त, सम्पूर्ण आत्म-तत्त्व हूँ।' समाध्यावस्था का आधार यही है। इस अवस्था को प्राप्त करके साधक अपनी आन्तरिक सत्ता पर मन एकाग्र करता है। यह एकाग्रता पूर्ण रूप से आन्तरिक एवं आध्यात्मिक है, जब कि अन्य प्रकार की एकाग्रता बाह्य है और उनका अभ्यास संसार के मायावी क्षेत्र में किया जाता है; क्योंकि साधक का पूर्ण ध्यान नश्वर पदार्थों में फँसा होता है। अतएव, आध्यात्मिक साधना अपने गुरु के पास बैठ कर सीखी जा सकती है। गुरु एवं शिष्य का शारीरिक रूप में सामीप्य सदा अनिवार्य नहीं है। तत्त्वज्ञानी गुरु के लिए यह सामीप्य सर्वथा आवश्यक नहीं है; परन्तु जिज्ञासु साधक के लिए गुरु का सामीप्य निःसन्देह वरदान-स्वरूप है। यदि यह सम्भव न हो तो भी गुरु पथ-प्रदर्शन कर सकता है। गुरु के निर्देशन के बिना ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिए तथा गुरु जो विधि बताता है, उसी का पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।
यह एक सामान्य प्रथा है कि सर्वप्रथम जब शिष्य ध्यान लगाने बैठता है तो अपने गुरु का ही ध्यान करता है। जब आपके अन्तर्मन में गुरु की प्रतिमा रम जाये तो उस पर अपने इष्टदेवता का अध्यारोपण करें और यदि आप वेदान्ती हैं तो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करें। गुरु का ध्यान करने के उपरान्त शनैः-शनैः गुरु के रूप के स्थान में अपने परम आदर्श को सामने ले आयें।
अतएव गुरु की विद्यमानता का भाव एवं प्रारम्भ में गुरु के रूप पर एकाग्रता ध्यान को सुचारु एवं सफल बनाने में अतीव सहायक है।
भक्तजन अपने इष्टदेव को ध्यान का लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे लोगों के सामान्यतया अपने ही ध्यान-श्लोक होते हैं। ध्यान-श्लोक में इष्टदेव के प्रति प्रार्थना अथवा उनकी स्तुति होती है जो देवता के स्पष्ट एवं सम्पूर्ण रूप को आपके समक्ष ले आती है। उदाहरण के लिए यदि आप शिव के उपासक हैं तो उनकी उपासना के कुछ विशेष श्लोक होंगे जो उनके रूप के साथ मृमछाला, त्रिनेत्र आदि का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार भगवान् विष्णु का एक श्लोक में वर्णन है, जिसमें वे पीताम्बर, गदा, कमल-पुष्प एवं चक्र धारण किये हुए हैं। भगवान् कृष्ण का रूप मन-मोहक, सस्मित और हाथ में बाँसुरी लिये हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक देवता के अपने-अपने ध्यान-श्लोक हैं। साकार रूप के ध्यान-योगियों के लिए ध्यान-श्लोक का जप ही प्रथम अभ्यास-क्रिया बतायी गयी है। बारम्बार जप करने से देवता का स्वरूप स्वतः ही मन की आँखों के सामने आ जाता है। तदुपरान्त श्लोक के स्थान पर गुरु-मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए। यह मन्त्र है भगवान् शिव के लिए 'ॐ नमः शिवाय', भगवान् कृष्ण के लिए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं भगवान् विष्णु के लिए 'ॐ नमो नारायणाय' इत्यादि।
अनन्यमनस्कता प्राप्त करने के हेतु मन्त्र जप अति सहायक एवं लाभकारी है। जप दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम यह है कि मन्त्र जपते हुए भगवान् के गुणों-जैसे तेजस्विता, ओज एवं अनन्त शान्ति आदि का चिन्तन किया जाये। मन्त्रों में दैविक गुणों से भरे हुए नाम होते हैं। सभी नाम, चाहे वे किसी भी रूप की अपेक्षा करें, अन्ततः जो अद्वितीय परब्रह्म है, उस परम सत्य के सूचक होते हैं। भगवान् शिव की उपासना सर्वोपरि सत्य की उपासना है। देवीपूजक देवी को परम सत्य के तुल्य मानते हैं। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वे एक विशेष रूप से प्रेम करते हैं और इस रूप को वे सदा परम सत्य ही मानते हैं, जो नाम-रूप-रहित, नित्य और अनन्त है। अतएव, नाम का जप करते हुए भी उस अद्वितीय स्वतः प्रभावपूर्ण परब्रह्म के गुणों को ध्यान का विषय बनाया जा सकता है। स्व-लक्ष्य पर मन को केन्द्रित करने का मन का यह एक ढंग है; परन्तु इसमें एक बात सदा स्मरणीय है कि आप किसी भी देवता की उपासना क्यों न करें, आप उस अद्वितीय परमात्मा की ही उपासना करते हैं। भगवान् कृष्ण अथवा भगवान् राम की उपासना सच्चिदानन्द की उपासना है। भगवान् राम की उपासना करते हुए उन्हें दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं लिया जाता। उनकी तो सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं विनाशकर्ता के रूप में पूजा की जाती है। यदि यह कहा जाये, 'आप तो दशरथ के पुत्र हैं' तो स्वतः ही मुख से यह भी निकलता है, 'आप सब लोकों को बनाने वाले हैं।'
परमात्मा के नाम का ध्यान करते समय यदि मन चंचल हो उठे तो उसी समय आन्तरिक और मानसिक जप करना छोड़ कर जोर से सुनने योग्य स्वर में जप करना आरम्भ कर देना चाहिए। जब ऐसा लगे कि मन इतस्ततः भटकने लगा है तो मन्त्र-जप उच्च स्वर में आरम्भ कर देना चाहिए। ऐसा करने से मन तत्क्षण ही संयत हो जायेगा; क्योंकि कर्णेन्द्रिय मन को वशीभूत करने में सहायक होती है। इतना करने पर भी यदि मन एकाग्र न हो तो आँखें खोल कर उस प्रतिमा पर केन्द्रित करनी चाहिए जिसे ध्यान में बैठने से पूर्व सामने रखते हैं। यदि आप वेदान्तमतावलम्बी हैं तो 'ॐ' लिख कर अपने सामने रख सकते हैं और तब मन को वश में करने में आप दूसरी इन्द्रिय, चक्षु की भी सहायता ले सकते हैं। ध्यान के समय मन को और अधिक वशीभूत करने के हेतु वे साधन-स्वरूप बन जाते हैं। इस प्रकार दृष्टि द्वारा भी मन को अपने लक्ष्य पर केन्द्रित करने का उसी प्रकार प्रयत्न कर सकते हैं जिस प्रकार ध्यान के द्वारा। मन में पुनः पुनः इष्टदेव के विविध रूपों का ध्यान करें। किंचित् समयोपरान्त वाणी से जप बन्द करके मानसिक जप करें। अन्ततोगत्वा मानसिक जप ही अधिक महत्त्वपूर्ण कहा गया है, किन्तु समय-समय पर कर्णेन्द्रिय द्वारा श्रवण योग्य जप मानसिक जप से अधिक प्रभावशाली होता है। यही कुछ युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा चंचल मन को ध्यान में लक्षित केन्द्र पर एकाग्र किया जा सकता है।
सफल एकाग्रता के लिए किंचित् अन्य युक्तियाँ बताते हैं।
यथासम्भव, ध्यान का समय निश्चित रखना चाहिए। इससे बहुत सहायता मिलती है। समस्त भौतिक पदार्थों में एक प्रकार का तालमेल है। सर्व पदार्थ एक विशेष काल-चक्र के अनुसार गतिशील हैं। सभी बस्तुएँ, चाहे अन्तरिक्ष की हों अथवा भूलोक की, प्राकृतिक नियम के अनुसार चल रही हैं। एक व्यवस्था है। ऋतुओं का आगमन यथाक्रम होता है। मानव-विकास के विविध रूप भी नियम का अनुसरण करते हैं। समयानुसार व्यक्ति के भाव भी परिवर्तित होते रहते हैं। प्रातःकाल भाव कुछ और होते हैं तो सायंकाल में कुछ और। यहाँ तक कि हमारा अन्तरंग भी एक चक्र-विशेष का अनुसरण करता है। जिसमें शनैः-शनैः विवेकशीलता द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ध्यान में भी मन कुछ विशेष नियमों का पालन करता है। ध्यानार्थ समय निश्चित करने के अतिरिक्त यदि आप यह भी धारण कर लें कि समय-विशेष पर इतने समय तक ध्यान में अवश्यमेव बैठना है तो आप जानते हैं क्या होगा ? शीघ्र ही समय की इस अविरत नियमितता के पुनरावर्तन से मन स्वतः ही ध्यान में प्रवृत्त होने लगेगा। भौतिक क्षेत्र में वैज्ञानिक इस तथ्य को प्रमाणित कर चुके हैं।
नियमित समय पर किंचित् निश्चित काल के लिए ध्यान में बैठने से मन भी ध्यान में प्रवृत्त होने लगेगा। समय नियत करने से एकाग्रता एवं ध्यान में बैठना सुगम हो जाता है। मानव-मन रहस्यमय है। यह इच्छाओं- अनिच्छाओं से युक्त होने के कारण सदा अपनी प्रकृति का दास बना रहता है। किंचित् विशेष पदार्थों का अभ्यस्त होने पर उन्हीं की ओर प्रवृत्त रहने लगता है। अतएव, मन के विचार-क्रम को नियन्त्रित करने के लिए केवल नियमित समय ही नहीं, अपितु नियत स्थान भी होना अनिवार्य है। स्थान परिवर्तित करते रहना उचित नहीं, इससे मन विक्षिप्त होता है। एक ही आसन में बैठना चाहिए। निश्चित है कि सदा आदर्श स्थिति तो नहीं हो सकती, परन्तु यदा-कदा जब भी सम्भव हो, इन आदर्शों का पालन करना चाहिए। यात्रा करने वाला एक व्यापारी इन आदर्शों का पालन नहीं कर सकता; परन्तु ऐसे लोग, जो अधिक यात्रा नहीं करते, जैसे अध्यापक, दुकानदार आदि ध्यानार्थ स्थान तो निश्चित कर ही सकते हैं। आसन की महत्ता एवं आवश्यकता के सम्बन्ध में पूर्व पृष्ठों में कहा जा चुका है। कोई भी आसन जिसमें आप अधिक समय तक बैठ सकें, ध्यानार्थ चुन सकते हैं। कुछ बाहह्य सहायता भी ली जा सकती है। बैठने के स्थान को यदि सुगन्धित धूप जला कर अथवा पुष्पों द्वारा मनोरम बनाया जाये तो मन को ध्यानावस्थित होने में सफलता मिलेगी। ध्यानाभ्यास के स्थानों में, मन्दिरों आदि में सुगन्धित धूप जलाने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सामान्यतया सुगन्धित धूप एवं रम्य पुष्प मन को तुरन्त ही सुखद वातावरण में ले जाते हैं और मन में विक्षेप नहीं होता। मन अन्तर्मुखी हो जाता है। तो ये हैं कुछ और तथ्य जो एकाग्रता एवं ध्यान के अत्यन्त अनुकूल हैं।
सर्वोत्तम यही है कि ध्यानार्थ पृथक् कक्ष रखा जाये जिसमें कोई प्रवेश न करे। आप भी केवल ध्यानार्थ ही उसमें प्रवेश करें। आप जिस कमरे में रहते हैं, वह आपकी विचार-तरंगों से प्रभारित रहता है और यदि आप ध्यानार्थ पृथक् कक्ष रखते हैं तो वह आपके ध्यान-स्पन्दनों से आपूरित रहेगा। एक पृथक् कक्ष जिसे ताला लगा कर रखा जाये, सबके लिए सम्भव नहीं है; प्रत्युत् कम लोग ही ऐसा कक्ष रख सकते हैं जिसमें बैठ कर वे ध्यान लगा सकें। उन्हें इसके लिए कमरे का ही एक कोना चुन लेना चाहिए और वहाँ बैठ कर केवल ध्यान ही करना चाहिए।
ध्यानार्थ आसन लगाने के उपरान्त तत्काल ही ध्यानाभ्यास कर देने की अपेक्षा कुछ समय तक शान्त चित्त बैठना हितकर है। सर्वप्रथम शान्त भाव में अधिगमन कीजिए। यदि कोई पदार्थ आपके मन को व्यग्र कर रहा है तो सर्वथा शान्त हो कर मौन बैठ जायें और विचारों के प्रवाह का एक मार्ग बनाने का यत्न करें। यह मार्ग व्यक्ति-विशेष की अपनी ही युक्ति अथवा साधना-विशेष द्वारा बनाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव का ज्ञान होता है और वह जानता है कि किस युक्ति द्वारा उसका मन परमात्मा में संलग्न रह सकता है। कुछ लोग हाथ जोड़ कर प्रणाम-मुद्रा द्वारा प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। कुछ अन्य लोग किसी मन्त्र अथवा प्रणव (ॐ) के मन्द-मन्द उच्चारण द्वारा ही मन को भगवान् की ओर मोड़ सकते हैं। कुछ लोग ध्यान का प्रारम्भ मन्त्र-विशेष के गान से करते हैं और उनका मन तुरन्त ही ईश्वरोन्मुख हो जाता है। अभ्यास द्वारा मन एकाग्न होने का अभ्यस्त हो जाता है।
इसके अतिरिक्त किसी भी भाषा में कोई भावोद्बोधक सस्वर जप ध्यान के लिए सहायक हो सकता है; परन्तु यह परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बँधे हुए क्रम का अनुसरण करने से मन एकाग्र होता है। मन को उद्विग्न करने वाले विकर्षक कार्य करने के पश्चात् यदि आप तत्काल ध्यानस्थ होना चाहेंगे तो मन विरोध करेगा। अतएव, पहले मन को उचित भावानुकूल बनाना अनिवार्य है।
मन को सबसे अधिक विचलित कौन करता है? लौकिक माया-जाल! अतः ध्यान में बैठने से पूर्व ऐसा सोचना एवं अनुभव करना चाहिए कि ब्रह्माण्ड कोई नहीं, संसार भी नहीं, कहीं कुछ नहीं। न सूर्य है, न चन्द्र और न ही यह संसार । विश्व को अपनी दृष्टि से दूर कर दो। फिर क्या रह जायेगा? कुछ भी नहीं। केवल आप हैं। अब धीरे-धीरे अपने अंग शीर्ष, मुखादि को, व्यक्तित्व को नकारने का यत्न करो। अब शेष क्या है? शून्य! सबसे पहले पार्थिव चेतना, पार्थिव विचारों तथा सांसारिक विचारों को नकारना चाहिए।
जब आप अनुभव करते हैं कि कहीं कुछ भी नहीं है, तब धीरे-धीरे मन में विचार लाना चाहिए कि केवल परमात्मा है। तत्पश्चात् गुरु के द्वारा उपदिष्ट परमात्मा के रूप के प्रति विशेष भाव मन में लाना चाहिए। यदि आप भक्त हैं तो मन में यह भाव रखें कि अस्तित्व दोनों का ही है- ध्येय और ध्यानी। वेदान्ती इस भाव से ध्यान में बैठें कि असीम अस्तित्व, अगाध शान्ति और अपार आनन्द का एक महत् विस्तरण है। सर्वत्र केवल शान्ति है, अन्य कुछ भी नहीं। ब्रह्म-तत्त्व के बोध से मन को भरने का यत्न करना चाहिए। यही दो तत्त्व, समस्त जगत् एवं स्वयं के अस्तित्व को भी नकार देना और परमात्मा की सत्ता को ही निश्चित रूप में अनुभव करना बहुत बड़े सहायक हैं। निरन्तर अभ्यास द्वारा साधक अचिरेण ध्यान-भाव में लीन होने लगता है; संसार का किंचित् मात्र भी ध्यान नहीं रहता और आत्म-तत्त्व परमात्म-तत्त्व के भाव में ही आनन्दित होने लगता है। यही अवस्था होती है ध्यान आरम्भ करने की।
ध्यान-मार्ग में अनेक विघ्न आ सकते हैं। ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु निद्रा है। द्वितीय महाशत्रु है मनोराज्य अथवा कल्पना के पुल बाँधना। ऐसा भी होता है कि ध्यान में बैठे हुए भी आप किसी कल्पना-लोक में विचरण कर रहे हैं और आपको इसका ज्ञान भी नहीं है। ध्यान का यह सबसे रहस्यमय भाग है और जब प्रकृत अवस्था में आने पर इस अवस्था का बोध होता है, तो आपको क्षोभ भी होगा कि आप क्या कर रहे थे? इस कल्पना-सौध-निर्माण के पीछे इच्छाएँ छिपी होती हैं, जिनका आपको ज्ञान नहीं है। वे क्षणिक सन्तुष्टि देने के लिए नाना प्रकार के चित्र उपस्थित करती हैं। आप जानते हैं कि कुछ सुख आध्यात्मिक जीवन के विरुद्ध हैं। अतः चेतन तत्त्व की सहायता न मिलने पर वे मन में प्रविष्ट होने लगते हैं।
आकांक्षाएँ ध्यान में बड़ा व्याघात पैदा कर देती हैं। यदि आपकी आकांक्षा एक ऐसा महान् योगी बनने की है जिसके बहुत से शिष्य हों तो यह आकांक्षा आपके लिए अति-हानिकारक हो सकती है। आकांक्षा एवं इच्छा आध्यात्मिक मार्ग में दो बड़े विघ्न हैं। यदि साधक इनसे दूर रहने का प्रयास न करता रहे तो उसके लिए ये दोनों विनाशकारी सिद्ध हो सकती हैं। उन्नत अवस्था में ये दोनों अर्थात् महान् बनने की आकांक्षा एवं इच्छाएँ जिनका आपने दमन किया है, साधना में विघ्न डालती हैं। इसलिए इनके प्रति सावधान और जागरूक रहना चाहिए। विविध उपायों द्वारा इन्हें वश में किया जा सकता है जिनमें कुछ विशेष उपाय इस प्रकार हैं-ईश्वर-प्रार्थना, गुरु के समक्ष सच्चे मन से आत्म-समर्पण एवं भगवन्नाम-जप का अभ्यास। भगवान् के नाम का जप एक प्रभावपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति है जिसके द्वारा साधक योग-साधना के आभ्यन्तर मार्ग की सब बाधाओं और विघ्नों का सामना कर सकता है तथा उनको विनष्ट भी कर सकता है। विश्वास और निरन्तर अभ्यास के बिना नाम-जप की शक्ति का अनुभव कठिन है।
उचित भाव द्वारा ही नाम-जप की शक्ति जाग्रत की जा सकती है। भाव से जितना अधिक जप किया जाये, उतनी ही अधिक शक्ति उत्पन्न होती है और अन्ततः एक ऐसा समय आता है जब नाम में निहित शक्ति पूर्ण रूप से जाग्रत हो उठती है। नाम की शक्ति सम्भावनाएँ लिये हुए सुप्त रहती है; परन्तु निरन्तर जप से मन्त्र-चैतन्य का बोध हो जाता है। नाम-शक्ति अणु-शक्ति से कई लाख गुणा अधिक प्रभावशाली है। नाम का जप भक्तिपूर्वक करना चाहिए। एकाग्रता और ध्यान में सफलता प्राप्त करने में यह अपरिहार्य एवं बड़ा सहायक है।
ध्यान
एकाग्रता प्राप्त करने के लिए चंचल मन को विषयों से विमुख करना आवश्यक है। जब तक यह विषय-विमुख नहीं होता, आप एकाग्र नहीं हो सकते। एकाग्रता की प्राथमिक अवस्था में मन को विषयों से समेटना अनिवार्य है और यदि आपने मन की रश्मियों (वृत्तियों) को एकत्र कर लिया तो आप एकाग्र होने का प्रयत्न कर सकते हैं। जब तक एकाग्रता तैलधारा के समान अविरत एवं अटूट न हो, तब तक इसका अभ्यास करते रहना आवश्यक है। अनवरत प्रयत्न, आस्था एवं इन सबसे अधिक विवेक अपेक्षित है। जिस प्रकार मन आपके साथ वंचना करता है, उसी प्रकार आप भी मन के साथ प्रवंचना कर सकते हैं। यदि आपको छलने के लिए मन के पास अनेक युक्तियाँ हैं तो आप भी मन को कई प्रकार से छल सकते हैं और नाना प्रकार की युक्तियों से उसे पथ पर ला सकते हैं।
बुद्धि के दो स्वरूप हैं-विषयाकार बुद्धि एवं विवेकात्मक बुद्धि। मन का एक स्वरूप विषयासक्त होना चाहता है और दूसरा स्वरूप जानना चाहता है कि उचित और अनुचित क्या है, नित्य एवं नश्वर क्या है? इसे विवेक कहते हैं। मन जिज्ञासा करता रहता है कि मैं यहाँ किस लिए हूँ? उसे यह पता लगाना है कि संसार का वास्तविक तत्त्व क्या है और जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्या है जो उसे प्राप्त करना है। मन का जो भाग इस खोज में प्रवृत्त रहता है, वह इन्द्रिय-विषयों में आसक्त मन के दूसरे भाग का विरोध करता है। इस प्रकार विषयासक्त एवं विवेकशील मन में परस्पर संघर्ष चलता रहता है।
प्रभु का नाम लेने, स्तुति करने, गुरु के समक्ष आत्म-समर्पण करने, सत्संगति में रहने आदि से जैसे-जैसे मन की निर्मलता को शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही वैसे आपको अधिकाधिक सफलता प्राप्त होती जाती है। चंचल मन संयत होने लगता है और जब ऐसा हो जाता है तो ध्यान अपने लक्ष्य पर निरन्तर लम्बे समय तक अटूट रूप में बना रहता है। जब आप अपने मन को अविरतरूपेण ध्यान-लक्ष्य पर केन्द्रित करने में समर्थ हो जाते हैं, तब आप ध्यान की सप्तम अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान योग की ओर उत्तरोत्तर ले जाने वाली अवस्थाएँ हैं। आप मन को शत विषयों पर केन्द्रित नहीं कर सकते। अतः विक्षेपावस्था में बाह्य-विषयों से मन को समेटना अनिवार्य है। विक्षेप दूर होने पर ही ध्यानावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ध्यानावस्था में पहुँचने तक मन को इन विविध अवस्थाओं द्वारा अनुशासित किया जाता है।
मन के पूर्णतया शुद्ध होने पर, आत्म-संयम प्राप्त होने पर और सात्त्विक बनने पर ध्यान लगाना कठिन नहीं है। केवल अभ्यास को तीव्र करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात् यह क्रम निर्विघ्न चलता रहता है। ऐसा आदर्श परिस्थितियों में ही होता है; परन्तु अधिकांशतः होता क्या है? प्रायः साधक कुछ पुस्तकों का अध्ययन करके ध्यान लगाने का प्रयास करने लगते हैं। ध्यान तो वस्तुतः साधना की लगभग अन्तिम अवस्था है। यह स्वर्ग-लोक का प्रवेश-द्वार ही है। यदि आप अकस्मात् ही शिखर पर पहुँचना चाहें तो कहीं के न रहेंगे। जिस क्षण भी आप ध्यान में बैठते हैं, आप सुन्दर मनोराज्य में पहुँच जाते हैं। आपको ज्ञात नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं? सहसा जब आप जागते हैं तो अनुभव करते हैं कि आप कल्पना के पुल बाँध रहे थे। परन्तु ऐसा क्यों होता है? इसका स्पष्टीकरण क्या है? आपके मन में अनेक आकांक्षाएँ और विषयासक्तियाँ निहित हैं। मन सर्वथा अशुद्ध है। उसमें सत्त्व नहीं है। अतः जब आप ध्यान में बैठते हैं, तब अधोमन ही क्रियाशील होता है। ध्यानावस्था का वास्तविक आरम्भ उस समय से होता है जिस समय से आप कायिक तत्त्व से ऊपर उठने लगते हैं। जब तक आप देह-चेतना का अतिक्रमण नहीं कर लेते, मन ध्यान में लग ही नहीं सकता।
मन का शुद्ध एवं विरक्त होना ध्यान के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अभ्यास की पूर्वावस्था में निर्मल मन की वैसी अवस्था नहीं होती। विषयों में आसक्त रहने पर आपको सफलता प्राप्त करना असम्भव है। कोई छोटी-सी बाधा भी आपको व्याकुल कर सकती है। व्याकुल (अस्थिर) मन से यदि आप अपने कक्ष में प्रवेश करेंगे तो वही (व्याकुल मन वाली) बातें फिर से मन में आयेंगी। दिन में जो-जो घटनाएँ घटीं, उन्हीं का स्मरण होता रहेगा; ध्यान नहीं होगा। हमारा शरीर से घनिष्ट सम्बन्ध है, मन और शरीर भी अलग नहीं किये जा सकते। यह सम्बन्ध कम भी नहीं हो सकता। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जब तक ध्यान की उच्चावस्था न प्राप्त कर लें, तब तक आप ध्यान आरम्भ ही न करें; क्योंकि ऐसा सम्भव ही नहीं है। आपका दृष्टिकोण सन्तुलित होना चाहिए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपके लिए करने योग्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कौन-सा है? निःसन्देह, ध्यान में अधिष्ठित होना ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है; परन्तु आरम्भिक अवस्था में ऐसा करना उचित नहीं। प्रारम्भिक अवस्था में तो संयम और सात्विक गुणों का विकास करना आवश्यक है।
जब तक आप मैट्रिक पास न कर लें, आप बी. ए. कक्षा के छात्र नहीं बन सकते। जब तक आप बी. ए. पास न कर लें, आप एम. ए. का प्रयास नहीं कर सकते। पहले मैट्रिक, फिर बी. ए., एम. ए. और उसके बाद ही पी-एच. डी. हो सकती है। आध्यात्मिक जीवन के आरम्भ में योग की कुछ पुस्तकें पढ़ कर लोग समझने लगते हैं कि ध्यान द्वारा बहुत शान्ति प्राप्त होती है और हर क्षेत्र पर इससे आधिपत्य प्राप्त कर सकते हैं। उनके विचार में ध्यान द्वारा ही आकर्षक व्यक्तित्व का विकास एवं सब वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। अतएव, वे सीधे ध्यान में लग जाते हैं। यह स्वाभाविक ही है, परन्तु यह विचार भी करना चाहिए कि ध्यान में बैठने योग्य बनने के लिए कौन-सी शर्तें पूरी करनी अनिवार्य हैं। सर्वप्रथम चरित्र-निर्माण आवश्यक है। इसके बिना ध्यान में बैठना समय नष्ट करना है; क्योंकि निद्रा आने लगेगी। ध्यानावस्था में अनिद्र रहना योगी के लिए अति-कठिन कार्य है। तमोगुण के प्रभाव से झपकी आने लगती है। आप एक प्रकार का स्वप्न-सा देखने लगते हैं या कल्पना के पुल बाँधने लगते हैं।
अतएव योग-मार्ग में अग्रसर होते हुए प्रारम्भ में दस या पन्दरह मिनट तक ध्यान में बैठना चाहिए; लेकिन पूरा बल प्रभु-गुण-गान एवं शास्त्राध्ययन आदि जैसी प्रारम्भिक अवस्थाओं पर देना चाहिए। ज्ञान और कर्मेन्द्रियों द्वारा किये जाने के कारण यह आपको सजग रखते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भी यह आवश्यक है। अभ्यास के साथ ध्यान का समय भी धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए।
आरम्भ में जब तक मन अशुद्ध होता है, योग की प्रारम्भिक अवस्थाओं पर जिनमें से हो कर आपको आना है, उचित ध्यान देना अत्यावश्यक है, अन्यथा ध्यान में सफलता प्राप्त नहीं होगी। जब तक आप कायिक बन्धन से युक्त हैं, तब तक काया-सम्बन्धी सभी अवस्थाएँ अथवा भाव मन पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अतः उस समय आपको सामान्य ज्ञान अथवा युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। एक सन्त ने कहा है, 'मन्त्र और यन्त्र का ही नहीं, तन्त्र का भी।' तन्त्र का अर्थ है कुशल परामर्श, कूटनीति। यह ज्ञात करना चाहिए कि बाधा कहाँ है और तब उसके अतिक्रमण का यत्न करना चाहिए। अपच होने पर ध्यान में बाधा आती है। रोग-चिकित्सा के लिए ध्यान का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके लिए चिकित्सक से पाचक दवा लेने की आवश्यकता होगी। थके होने पर भी मन को एकाग्र करना कठिन है। ऐसी अवस्था में कुछ विश्राम करना होगा। आपका सामान्य ज्ञान ही बतायेगा कि आपको कितने विश्राम की आवश्यकता है। वायु उत्पन्न करने वाला भोजन करने पर अथवा अयुक्ताहार करने पर ध्यान नहीं लग सकता। भिन्न-भिन्न लोगों में भिन्न-भिन्न भोज्य-पदार्थ वायु उत्पन्न कर सकते हैं। अतएव उचित आहार का चयन आपको स्वयं ही करना है।
कभी-कभी आप उदास एवं निराश से हो जाते हैं। किसी के साथ कलह होने पर भी उदासी आ सकती है। सुबह जागने पर पूर्व-संस्कारों के कारण आप निराश हो सकते हैं। यदि आपके मन में निराशा की भावना है तो मन ध्यान में नहीं लगेगा। यदि आप गायक हैं तो कोई भक्तिगीत गायें या कुछ अधिक दूर तक भ्रमण के लिए निकल जायें।
प्राकृतिक वातावरण में यदि आप लम्बे भ्रमण के लिए चले जायें तो आपका चित्त अद्भुत रूप से प्रसन्न हो जायेगा। कोई मनोरंजक पुस्तक या लेख पढ़ें। सुन्दर उद्यान में घूमें। मन की निराशा दूर करने के लिए इस तरह की विवेकपूर्ण युक्तियों से काम लें। शारीरिक कष्ट होने पर भी ध्यान नहीं लगता। कष्ट-निवारण के लिए शरीर में मालिश अथवा सेंक की जा सकती हैं।
यह सब इसलिए बताया जा रहा है; क्योंकि सामान्यतया लोगों में ऐसा देखा गया है कि शारीरिक अवस्था का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और मन ध्यान से हट जाता है।
यदि आप ध्यानस्थ हो जायेंगे तो ऐसी अवस्था में आप शरीर को भूल जायेंगे। तब इन सब बातों की चिन्ता आवश्यक नहीं है। परन्तु ऐसी अवस्था प्राप्त करने तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। ये सब विघ्न-स्वरूप हैं और इनका त्याग कर देना ही सर्वोत्तम है। ध्यान से पूर्व कभी भी अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन, जो आपके शरीर एवं मन के अनुकूल न हो, नहीं करना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शरीर में अत्यधिक थकान, उदासीनता एवं पीड़ा हो। मन शान्त न हो तो आप ध्यानस्थ नहीं हो सकते। आपका मानसिक सन्तुलन समान रहना चाहिए। सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। वैराग्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वैराग्य न होने पर मोह-माया मन के सन्तुलन को बिगाड़ देंगे। अतएव इच्छा, काम, क्रोध आदि का निराकरण अनिवार्य है। एक वर्ष की अवधि में उनका निराकरण नहीं हो सकता। कदाचित् दस वर्ष भी लग सकते हैं; परन्तु अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए।
साधक की संलग्नता का एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण महाभारत में समुद्र तट पर रहने वाले उस पक्षी के दृष्टान्त से मिलता है जो अपनी नीड़ की रक्षा हेतु अपनी चोंच द्वारा सागर को रिक्त करने के लिए कटिबद्ध था; कृत-संकल्प था। इसी प्रकार आध्यात्मिक अभ्यास जन्म-जन्मान्तर भी चल सकता है। इस जन्म में अन्तिम श्वास तक हमें उद्यम करते रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको संकल्प कर लेना चाहिए कि फल की इच्छा किये बिना आप हर दशा में उद्यम जारी रखेंगे। आप प्रयत्नशील रहेंगे तो सफल होंगे। मन में धारण किया हुआ अत्यल्प सुविचार, प्रभु-गुण-गान का केवल एक अवसर अथवा एक बार भी सत्य पर दृढ़ रहना। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए किंचित्-सी चेष्टा-यह सब सायास एकत्र होते रहते हैं और इस एकत्र होने के परिणाम-स्वरूप अन्ततः अन्तर्चक्षु खुल जाते हैं। एकत्रित लाभ चक्षुओं से दिखायी नहीं पड़ता। इस लाभ द्वारा व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है, उसे केवल ब्रह्मज्ञानी देख सकता है; व्यक्ति स्वयं नहीं देख सकता। अतः आपकी अनवरत चेष्टा वज्र समान होनी चाहिए।
दिन-प्रतिदिन जैसे-जैसे आप अभ्यास करेंगे, सभी बाधाएँ दूर होती जायेंगी और आप शारीरिक तल से ऊपर उठ जायेंगे एवं तदुपरान्त मानसिक तल से भी ऊपर उठ जायेंगे। उच्चतर बोध के उदय होने पर, जब आप शुद्ध मन में अधिष्ठित हो जाते हैं, तब थोड़े समय ध्यान में बैठना भी असीम आध्यात्मिक शक्ति देता है। और अग्रसर होने पर ध्यान गहन हो जाता है तथा आप राजयोग की अष्टम और अन्तिम अवस्था के लिए तैयार हो जाते हैं। यह अत्युत्तम परमचेतनावस्था है। पारिभाषिक शब्द में इसे समाधि कहा जाता है।
मन एवं उसके नियन्त्रण-सम्बन्धी कुछ और तथ्य
अब हम मन की प्रकृति और उसके व्यवहार की कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण अवस्थाओं और मन को धीरे-धीरे वश में करने की एवं उसे उत्तरोत्तर एकाग्रता के लिए यथायोग्य बनाने की कुछ अनुभूत और प्रभावशाली विधियों का विवेचन करेंगे।
मन की प्रकृति के बारे में ज्ञातव्य प्रथम बात यह है कि मन आदतों का दास है। मन सदा आदत के अनुसार बने हुए हमारे विचारों का अनुकरण करता है। पुनः-पुनः आने वाला विचार मन की प्रकृति बन जाता है। मन को संयत करने में यत्नशील साधक को मन की इस वृत्ति को कदापि नहीं भुलाना चाहिए। मन के इस विशेष स्वभाव का अब हम अधिक स्पष्ट रूप से और विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे।
डाक्टर बनने का इच्छुक विद्यार्थी जब निरन्तर छह वर्ष पर्यन्त मेडिकल कालेज में अध्ययन कर लेता है तो उसके मन में सदैव रोग, औषधियाँ और भेषजशास्त्र ही घूमते रहते हैं। उसके अचेतन मन में स्वतः ही औषधियों और रोगियों के विचार भर जायेंगे और यह विचार पुनः पुनः केन्द्र की ओर लौट कर आयेंगे। उसमें अन्य बातों के बारे में विचार करने की क्षमता कम होगी और चिकित्सा व्यवसाय का ध्यान करने की अधिक। अविरत रूप से फौजदारी, दीवानी मुकदमों, कानून, कचहरियों और न्यायाधीशों के विचारों में मन लिप्त होने पर क्या होगा? मन एक ऐसे विशेष स्वभाव में लीन हो जायेगा जिसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से केवल इन्हीं विचारों को ग्रहण करने की होगी। शोक और अपराध का चिन्तन करना ही इसकी प्रवृत्ति हो जायेगी। इंजीनियरिंग या किसी और व्यवसाय में भी यही होता है। एक इंजीनियर का मन गणित में संलग्न रहता है और उसका सम्पूर्ण जीवन इसी में ढल जाता है। इस प्रकार उसका मन यन्त्र-शास्त्र निरत हो जाता है। यदि वह यन्त्र-शास्त्र से भिन्न अन्य पदार्थ का चिन्तन करे तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा।
यदि एक चिकित्सक साधक भी है और ध्यान में बैठता है तो उसके मन को विक्षिप्त करने वाले विचार सदा अस्पतालों, रोगियों आदि के ही होंगे। इसी प्रकार एक व्यापारी जब योगाभ्यास करने का यत्न करेगा तो व्यवसाय में लाभ और हानि एवं बाजार के मोल-भाव उसे विक्षिप्त करेंगे।
इससे अब मन को वशीभूत करने और एकाग्रता में सफलता प्राप्त करने का निश्चित सूत्र मिल गया है। वह सूत्र कौन-सा है? अपने कार्यशील जीवन की साधारण दिनचर्या के समय भी आप मन को ध्यान के वस्तु-विषयक विचारों में निरत रखने का यत्न करें। एक भक्त अपने मन को नियन्त्रित तथा लक्ष्य-जैसे राम, कृष्ण, शिव, देवी, ईसामसीह या अल्लाह-पर एकाग्र होने के हेतु अपने अभ्यास को ध्यान के नियत समय में ही सीमित नहीं रखेगा। प्रातः-सायं ध्यान में बैठने के अतिरिक्त भी दिन-भर मन को ध्यान के विषय के विचारों से ओत-प्रोत रखना चाहिए। भक्त को निरन्तर अपने इष्ट का स्मरण करते रहना चाहिए-इष्टदेव चाहे भगवान् राम हों, भगवान् कृष्ण अथवा अन्य कोई देवता। ईसाई लोग ईसामसीह का मनन कर सकते हैं। किसी भी क्षण 'उसे' भुलाना नहीं चाहिए। केवल प्रार्थना के नियत काल में ही अपने इष्ट का स्मरण एवं मनन अनिवार्य हो, ऐसा नहीं है। दैनिक व्यवहार में भी उसका विस्मरण नहीं करना चाहिए। ध्यान-प्रवाह सदैव रहना चाहिए। क्रियाशील जीवन में भी उसे बनाये रखना अनिवार्य है। यह मनन उतना कार्यशील एवं गहन तो नहीं होगा जितना ध्यान के समय में होता है, फिर भी इसे अविरतरूपेण चलते रहना चाहिए।
आपने थीसेस की कहानी सुनी होगी। वह एक बीहड़ स्थान (भूल-भूलैया) में गये, जहाँ एक राक्षस रहता था। उन्हें राक्षस का वध करके वापस आना था। वह कुटिल मार्ग ऐसा था जहाँ पहुँच कर कोई वापस नहीं आ सकता था। उनके एक मित्र ने उन्हें धागे का एक गोला दिया और कहा: 'उस स्थान पर जाओ जहाँ राक्षस निवास करता है; परन्तु जैसे-जैसे आप आगे बढ़ो, इस धागे के गोले को खोलते जाओ। बस, क्रम टूट गया तो वहाँ से वापस आना सर्वथा असम्भव होगा।' उन्हें यह युक्ति बतायी गयी। उन्होंने ऐसा ही किया और वे राक्षस का वध करके वापस लौटने में सफल हो गये।
इसी प्रकार ध्यान-सूत्र भी रखना चाहिए। प्रातःकाल जब आप मन एकाग्र करते हैं तो ध्यान की धारा बनाये रखिए। दोपहर को पुनः जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो वही धारा चलती रहेगी। निद्रा में भी ध्यान का यह क्रम अर्धचेतन मन में चलता रहता है। इसकी प्रतीति तब होती है जब स्वप्नावस्था में ध्यान-प्रवाह आ कर स्वप्न को परिवर्तित कर देता है।
योग आरम्भ करने से पूर्व यदि दुःस्वप्न आयें तो उस समय भगवान् का चिन्तन आरम्भ कर देना चाहिए। दुःस्वप्न कम आने लगेंगे और कम प्रभाव डालेंगे; क्योंकि अकस्मात् ही स्वप्न में यह विचार आ जाता है कि भगवान् तो निरन्तर मेरे साथ हैं, मेरे पास कोई और नहीं आ सकता। स्वप्नावस्था में भी इसी अटल आस्था का अनुभव किया जा सकता है। जो अनुभव आपको भयभीत कर रहा था, वह शक्तिहीन हो कर चला जायेगा। इससे एक रहस्यपूर्ण तथ्य का उद्घाटन होता है कि स्मरण-श्रृंखला निद्रावस्था tilde pi अथवा स्वप्नावस्था में भी टूटती नहीं। कभी-कभी तो स्पष्ट रूप से ही इसका आभास होता है।
जाग्रत, स्वप्न तथा निद्रा अवस्थाओं में ध्यान-श्रृंखला के सतत रूप से चलते रहने के कारण यह श्रृंखला बनी रहती है और मन का एक भाग अपना साधारण कार्य करने में निरत रहता है। चारों योगों में इस कला की दक्षता का प्रमाण मिलता है। ज्ञानी लोगों ने ध्यान करने की भिन्न-भिन्न युक्तियाँ बतायी हैं। वेदान्तियों के अनुसार इसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं। वे निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, चाहे वे ध्यान के लिए आसन लगाये हों अथवा कार्य-निरत हों, वे यही विचार मन में रखते हैं कि वे ब्रह्म-स्वरूप हैं। इसे ब्रह्म-चिन्तन भी कहते हैं।
वास्तविक ध्यान एवं ध्यान की अविरत धारा बनाये रखने में कुछ अन्तर नहीं है। ध्यान गहन एवं सूक्ष्म होने के अतिरिक्त इन्द्रियों के विषयों से इतना विमुख हो जाता है कि इन्द्रियाँ बाह्यतः कार्यशील नहीं रह जातीं और मन ध्यान में विलीन हो जाता है, परन्तु यह चिन्तन इन्द्रियों के पूर्ण संहरण से युक्त नहीं होता। इन्द्रियाँ बाह्य पदार्थों को देखती रहती हैं और आप भी बाह्य विषयों में घूमते रहते हैं; परन्तु मनन चलता रहता है। इसे आत्म-चिन्तन भी कहते हैं। यह अति-प्रभावपूर्ण उपाय है; क्योंकि यह मन के उसी स्वभाव को जाग्रत करता है जिसमें यह जाग्रतावस्था में निरन्तर निरत रहना चाहता है अथवा उसमें प्रवृत्त होता है। ध्यान-विषय की स्मृति निरन्तर बनाये रखने से क्या होता है? चिन्तन उसी प्रकार होता है जैसे चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी, वकील अथवा इंजीनियर के मन में अपने-अपने विषय के सम्बन्ध में होता है।
यदि आप ध्यान के लिए बैठें तो क्या विचार आपके मन में आयेंगे ? वही विचार तो आयेंगे जिनका दिन-भर आप चिन्तन करते रहे; परन्तु यह चिन्तन किसका था ? भगवान् का ही, जो ध्यान का विषय है। अतएव ध्यान के अभ्यासी को इस प्रक्रिया को उत्तरोत्तर बढ़ा कर एक ध्यान-विधि बना लेनी चाहिए।
भक्त अपने भगवान् का स्मरण प्रतिक्षण करने का यत्न करता है। वह अपने इष्टदेव के नाम का मानसिक जप करता है। यदि वह भगवान् शिव का भक्त है तो चाहे वह घूम रहा हो अथवा कुछ श्रवण कर रहा हो, शारीरिक कार्य कर रहा हो, 'ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय' का मानसिक जप उसके मन में सदा चलता रहेगा। भगवान् राम का भक्त उन्हीं का नाम-स्मरण करता रहेगा। ये कुछ युक्तियाँ हैं जिनसे मन अपनी उस ध्यान-वस्तु में ही निविष्ट रहता है जिसका वह योगाभ्यास के क्षणों में ध्यान करता है। योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए, ध्याता के लिए जो इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, यह (युक्ति) अमूल्य है।
जप के अतिरिक्त एक अन्य युक्ति, जो निरन्तर स्मरण के लिए लाभकारी है- वह है प्रत्येक पदार्थ में भगवान् का ही रूप देखना। उदाहरणतया, राम का भक्त केवल इस भाव से मन को समस्तरूपेण राममय बनाने की चेष्टा करता है कि जो कुछ भी वह देखता है, स्वाद लेता है अथवा श्रवण करता है, सब राम ही राम हैं। ऊपर, नीचे, दायें, बायें-सर्वत्र राम ही हैं। मेघ (बादल) राम हैं। वृक्ष राम हैं। वह सर्वत्र राम को ही देखता है। संसार के सब पदार्थ-चर या अचर, राम हैं। वह प्रत्येक वस्तु में केवल राम का ही प्रत्यारोपण करता है और इस प्रकार उसके लिए संसार में सब-कुछ राममय बन जाता है। यहाँ प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी की पंक्ति याद आती है-
सिया राममय सब जग जानी।
करहुँ प्रणाम जोर जुग पानी।।
वायु में, पानी में, अन्तरिक्ष में, श्वास में, प्रत्येक पदार्थ में उन्हें राम ही राम दृष्टिगोचर होते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय में भी यही वर्णित है। भगवान् सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी हैं। भगवान् अर्जुन को अपने विश्व-रूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन सर्वत्र, सर्वशक्तिमान् आत्म-तत्त्व का ही दर्शन करते हैं। भगवान् को छोड़ कर अन्य कहीं कुछ भी नहीं है। इसे विश्व-रूप-दर्शन कहते हैं। मन जब स्वतः ही इस रूप को ग्रहण करने की ओर प्रवृत्त होने लगे तो इस अद्भुत भावना से मन को पूर्णतया उसी रूप-रंग में रंगा जा सकता है। यह अभ्यास दृढ़ हो जाने पर इन्द्रियाँ भगवान् से दूर नहीं होंगी, चाहे वे कहीं भी विचरण करती रहें।
यदि साधक किसी पदार्थ पर दृष्टिपात करता है तो उसमें भी उसे भगवान् ही दिखायी देते हैं। चक्षुर्विषय कुछ भी हो, उसमें उसे भगवान् ही सामने दिखायी देंगे। वह श्रवण भी करता है तो भगवान् का नाम ही श्रवण करता है। इन्द्रियाँ कहीं भी जायें, भगवान् की ओर ही प्रवृत्त होंगी। अतः साधक को इन्द्रियाँ कुपथगामी नहीं बनातीं। वे उसे भगवान् से सम्पर्क बनाये रखने में सहायता ही देने लगती हैं। समस्त प्रकार के विक्षेपों का उन्मूलन करने के हेतु यह अद्भुत उपाय है; क्योंकि साधक को सर्वतः भगवान् ही दृष्टिगोचर होते हैं और उसका बाह्य जीवन भी ब्रह्म-चिन्तन में श्रृंखलाबद्ध हो जाता है। सिक्ख लोग भी इसी नाम-स्मरण को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं।
स्व-लक्ष्य (अर्थात् भगवान्) की प्राप्ति हेतु कर्मयोगी की मानसिक एवं भावुक प्रवृत्ति उसे निरन्तर प्रभु की व्यापकता का अनुभव कराने में सहायक रहती है। कर्मयोगी में यह भावुक प्रवृत्ति स्वतः उत्पन्न होती है; क्योंकि भगवान् को देखे बिना उसकी पूजा कैसे की जा सकती है? आप भगवान् के दर्शन करने में असफल रह सकते हैं; परन्तु यदि आप केवल भगवान् को ही देखने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आप जानते हैं क्या होगा ?
कर्मयोगी निरन्तर स्मरण से, भक्त नाम-चिन्तन से, ज्ञानयोगी सर्वव्यापक प्रभु का ध्यान करने से एवं राजयोगी प्रत्याहार में मन का अधिष्ठान करने से मन की विचारधारा को परिवर्तित कर लेता है। राजयोगी को मन एकाग्र करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होगी। प्रत्याहार की अवस्था उसमें अधिष्ठित हो चुकी है। मन को बाह्य विषयों से समेटने की कला में वह पारंगत हो चुका है। प्रत्याहार में समस्तरूपेण अधिष्ठित होने के उपरान्त वह एकाग्रता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार प्रत्याहार द्वारा राजयोगी का मन बाह्य विषयों में प्रवृत्त नहीं होगा; चाहे वह कार्य भी क्यों न करता रहे; क्योंकि उसके दृष्टिकोण में अन्तर आ चुका है। बाह्य पदार्थ उसके लिए छाया के समान हो जाते हैं।
राजयोगी प्रत्याहार द्वारा, भक्त स्मरण एवं मानसिक जप द्वारा, कर्मयोगी प्रार्थना-भाव एवं वेदान्ती ब्रह्म-चिन्तन द्वारा मन की चिन्तन करने की प्रवृत्ति को ही परिवर्तित कर सकता है। मन में 'चिन्तन' का नवीन स्वभाव बनाया जा सकता है। लौकिक विषयों का चिन्तन करने के स्थान पर साधक प्रभु-चिन्तन करने लगता है। ऐसा स्वभाव बन जाने पर ध्यान के समय आने वाले प्रतिकूल विचारों का साधक पर प्रभाव क्रमशः कम होने लगता है। वे धीरे-धीरे क्षीण होने लगते हैं तथा एकाग्रता की ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें सभी विचार (भाव) एकाग्रता और ध्यान के विषय की प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं। अतएव वे मन को विचलित करने का कारण नहीं बनते। क्षण-भर के लिए चाहे वे एकाग्रता की गम्भीरता को कम कर दें, लेकिन तत्काल ही ध्यान पूर्ववत् गहन हो जायेगा। ध्यान-प्रवाह अखण्ड रहता है, कभी मन्द हो सकता है; परन्तु टूटता नहीं। भक्त, वेदान्ती, कर्मयोगी अथवा राजयोगी-आप कुछ भी हों, यह अभ्यास निरन्तर करते रहना चाहिए।
राग और द्वेष
राजयोगी कहते हैं कि राग और द्वेष ऐसे संवेग हैं जो मन को सर्वाधिक विचलित करते हैं। मन में प्रविष्ट होने पर इनकी प्रवृत्ति बने रहने की होने के कारण यह मन का सन्तुलन बिगाड़ देते हैं। ये घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, असहनशीलता एवं चिन्ता के भावों का रूप धारण कर लेते हैं। ये सभी विचार संवेगों से घनिष्ट रूप से गुँथे हुए होते हैं। शुद्ध विचार, जो संवेगों से सम्बन्धित न हों; योग में विघ्न-रूप नहीं बनते। संवेग-रहित निरपेक्ष विचार भी आपको विचलित नहीं करते। मन को जितनी अधिक मात्रा में भावुकता, संवेग और भावनाएँ विचलित करते हैं; उतना बौद्धिक चिन्तन नहीं। भावुकता और भावों से मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। एक साधारण दृष्टान्त प्रस्तुत है-यदि आपके पास कोई मेज हो और उस पर धूल-मिट्टी आदि पड़ जाये तो आप बड़ी सुगमता से इसे साफ कर सकते हैं। झाड़न से पोंछने पर धूल हट जायेगी; परन्तु यदि मधु की एक बूँद गिर जाये तो झाड़ने-पोंछने पर भी मेज स्वच्छ नहीं होगी। पाउडर अथवा कोई भी सूखी वस्तु सुगमता से पोंछी जा सकती है। इसी प्रकार बौद्धिक विचार सुगमता से दूर किये जा सकते हैं; परन्तु यदि ये ही विचार भाव-प्रधान हो जायें तो इन्हें मन से निकालना दुष्कर है। मन इन विचारों से मुक्त होना चाहे तो भी हृदय साथ नहीं देता। संवेगों का निराकरण अत्यन्त कठिन है। शुष्क बौद्धिक विचारों की अपेक्षा इनका निराकरण अधिक कठिन है।
भय, ईर्ष्या, घृणा, असहनशीलता-ये सब सांवेगिक मनोविकार हैं। ये मन से सुगमतापूर्वक नहीं निकलते। हम भिन्न जातीय लोगों के मिले-जुले समाज में विचरण करते हैं। यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो जाये तो आप क्रोधित हो उठते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष आ जाये जो आपको प्रिय नहीं है तो आपके मन में घृणा-भाव उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति समभाव में संस्थित नहीं है, वह बड़े उत्तेजित स्वभाव का होता है। जब सार्वजनिक जीवन में हमें दुर्जनों तथा उन लोगों के मध्य भी रहना पड़ता है जो आध्यात्मिकता में हमसे नीचे स्तर पर हैं, तब हमारे मन में घृणा-भाव उत्पन्न हो जाता है। अपने समान लोगों के मध्य विचरण करना होगा। यदि कोई आपका मित्र है तो मित्र होने पर भी आप नहीं चाहते कि वह आपसे अधिक महान् हो। ऐसे अवसर पर मन ईर्ष्या आदि से भर जाता है, परन्तु यह क्षुब्ध करने वाला भाव समान लोगों के प्रति मन में उत्पन्न होता है। अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति एक-दूसरे प्रकार का ईर्ष्या-भाव मन में आ जाता है और हम मन में कहते हैं- 'यह लोग हमसे श्रेष्ठ क्यों हैं? जो पद उन्हें प्राप्त है, वह हमें क्यों नहीं प्राप्त ?'
निर्धन धनी से ईर्ष्या करेगा। किसी विद्वान् को देख कर कम बुद्धि वाला आपे से बाहर हो जाता है। कोई सोचता है कि इतनी लोक-प्रशंसा मुझे भी मिलनी चाहिए थी। यदि आप मन के इन भावों के शिकार हो जायें तो आप निरन्तर इन्हीं भावों से सन्तप्त रहेंगे।
इस संसार में अनेक द्वन्द्व हैं जैसे शीतोष्णता, आदर एवं निरादर आदि। अतएव बहुधा मन सन्तुलित न रह कर निरन्तर उद्विग्न रहने लगता है। सामान्यतया प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में संवेगों का अनुभव करता ही रहता है जिनके कारण वह सदा एक ऐसी अप्रिय स्थिति में रहता है कि मन एकाग्र नहीं हो पाता। अतएव, पूर्वजों ने सूत्र बताया है कि योगी को समाज में किस प्रकार रहना एवं विविध प्रकार के लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि हर समय आप दुष्कर्म होते देखते हैं अथवा दुष्ट लोगों को देखते हैं तो आप स्वयं से पूछेंगे - 'ऐसे दुष्ट लोग संसार में क्यों हैं?' मन का सन्तुलन नहीं खोना चाहिए। अपने समान लोगों के प्रति मित्रभाव रखें और अपने से साधारण लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव। निम्न वर्ग के लोगों के मध्य आपका हृदय पिघल जाना चाहिए। कोई पद, आयु अथवा वैभव की दृष्टि से आपसे छोटा होता है। करुणार्द्र (दयाशील) होने पर आप दूसरे की सब कमियों को सहन कर लेंगे। अपने से बड़े लोगों के समक्ष शान्त एवं प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। वे कैसे भी हों, आप शान्त रहिए। उनके समक्ष प्रसन्न रहिए। विपरीत द्वन्द्वों में आपका कैसा व्यवहार उचित है?
भर जाने दो इस संसार को द्वन्द्वों से। उन पर ध्यान ही न दो। आपको उनके प्रति चिन्ता नहीं होनी चाहिए। भगवान् प्रत्येक वस्तु का ध्यान रखता है। अतः इस प्रकार की मैत्री, करुणा एवं उदासीनता का अभ्यास करना चाहिए। इन सबका अभ्यास करने से मन शान्त हो जाता है एवं इसके अन्दर से घृणा, असहनशीलता एवं स्पर्धा के भावों का निराकरण हो जाता है। यही सर्वोत्कृष्ट कला है जो पुरातन ऋषियों ने हमें सिखायी है।
ध्यान के लिए पूर्वाकांक्षित योग्यताएँ
आपको इस बात का ज्ञान तो हो ही गया है कि ध्यान से पूर्व नींव-स्वरूप सात्त्विकता, आत्म-संयम, इन्द्रिय-संयम एवं वैराग्य में अधिष्ठान कितना महत्त्वपूर्ण है। बाह्य विषयों के आकर्षण का झुकाव मन को अन्तर्मुख होने से रोकता है। सदाचार, संयम, यम, वैराग्य-इन विषयों का वर्णन इसलिए किया गया कि यदि इन प्रारम्भिक गुणों का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया जाये तो मनुष्य की शारीरिक प्रकृति और नैतिक वृत्ति सम्यक् रूप से प्रशिक्षित एवं शुद्ध हो सकती हैं। ऐसा साधक संयत, सदाचारी और जितेन्द्रिय बनता है। तब उसके लिए उच्चतर, सूक्ष्मतर लक्ष्य पर मन को एकाग्र करना और ध्यान लगाना सहज हो जाता है। इन प्राथमिक विषयों का अभ्यास किये बिना अकस्मात् ही यदि ध्यान आरम्भ किया जाये तो यह अतीव कठिन कार्य बन जायेगा और मन के साथ अन्तहीन संघर्ष करने में अधिक शक्ति लगेगी; क्योंकि निम्न प्रकृति पूर्णतया परिवर्तित नहीं हुई है। अयोग्य होने पर भी आप ध्यान लगाने का यत्न करेंगे तो इसका परिणाम प्रतिकूल होगा। फल-स्वरूप मन के असन्तुलन एवं अवसाद का सामना करना पड़ सकता है; क्योंकि निम्न प्रकृति का अभी निराकरण नहीं हुआ। वह अभी विद्यमान है, उसमें परिवर्तन नहीं आया। और यदि केवल दृढ़ निश्चय एवं संकल्प द्वारा ही आप मन को ध्यानस्थ करने का यत्न करेंगे तो अन्तःकरण में द्वन्द्व के कारण अनेक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।
अनेक साधक, जिनकी आध्यात्मिक विज्ञान में अधिक पहुँच है और जो मौन धारण कर लेते हैं एवं हठ द्वारा ध्यान लगाने का यत्न करते हैं; कामेच्छाओं से उनकी स्नायविक शक्ति क्षीण होती रहती है जिनके कारण उनका अध्यात्म-सम्बन्धी समायोजन उचित प्रकार से नहीं होता और साधक विलक्षण एवं सनकी होने लगते हैं। जो साधक अपने स्वभाव को अनुकूल किये बिना ही ध्यान लगाने का हठपूर्वक यत्न करते हैं, उनमें अनेक आध्यात्मिक विषमताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। परन्तु साधक को यह ज्ञात कैसे हो कि वह उचित पथ पर चल रहा है अथवा नहीं? इसके लिए गुरु. से परामर्श लेना सदा हितकर है। यह सार्वभौम तथ्य है कि अपने प्रति प्रत्येक व्यक्ति अच्छी धारणा रखता है। प्रत्येक यही समझता है कि वह ध्यान लगाने के योग्य है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं को सबसे महत्त्वपूर्ण (गौरवशाली) व्यक्ति मानना बड़ा स्वाभाविक है; परन्तु यह स्वाभाविक दुर्बलता साधना में विघ्न-स्वरूप नहीं होनी चाहिए। सदा गुरु की छत्र-छाया में रहना चाहिए। सावधानी से ध्यान-मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। साहसी, परन्तु अवेक्षित होना अनिवार्य है।
निष्काम सेवा द्वारा असाधु से साधु-स्वभाव बनने का यत्न चाहिए। मन शुद्ध करने के लिए अविरत रूप से निष्काम भाव से ही सेवा करनी अनिवार्य है। सब प्रकार की अपकृष्ट सेवा भी करनी चाहिए। मन की शुद्धि के लिए जो व्यक्ति इसे यौगिक अंग समझ कर कार्य करता है, उसके लिए कोई भी कृत्य नीच नहीं है। रोगियों की शैया का पात्र धोना चाहिए। द्वारपाल जब भोजन करने जायें तो उनके जूते साफ करने चाहिए। उस समय मन में ऐसा भाव रखना चाहिए जैसे आप भगवान् की पूजा कर रहे हों। यह कार्य पूर्ण भाव एवं नम्रता से करना चाहिए। इस निष्काम सेवा से अहंभाव कम होता है। बड़प्पन की भावना का पूर्णतः निराकरण करने हेतु सब प्रकार की सेवा करनी चाहिए। अपनी सुख-सुविधाओं का उत्सर्ग कर देना चाहिए। तब ही आप आत्मोत्सर्ग की भावना से युक्त हो सकते हैं। यह सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक करने चाहिए। ऐसी भावना रखनी चाहिए कि आप सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा भाव रखिए, 'प्रभु-कृपा से मुझे प्रसाद-रूप में यह सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, वैसे मैं इस अवसर को प्राप्त करने योग्य कदापि नहीं था।'
अत्यन्त नम्रता के इस भाव से सेवा करनी चाहिए- 'मैं यह करने योग्य नहीं हूँ; परन्तु प्रभु की कृपा से मुझे यह सेवा करने की अनुमति प्राप्त हुई है।' प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई आ कर आपको काम के लिए आवाज दे। सेवा का अवसर ढूँढ़ना चाहिए। इस प्रकार की सेवा से हृदय पवित्र होता है और जब हृदय पवित्र हो जाता है, ध्यान स्वतः होने लगता है।
ध्यान का प्रभाव प्रतिकूल अथवा इच्छा के विरुद्ध न हो, इसके लिए निष्काम सेवा द्वारा पवित्रता की महत्ता बतायी गयी है। साधना में बहुत आगे बढ़े हुए साधकों के मन में भी न्यूनाधिक संघर्ष रहता ही है; परन्तु ऐसा तभी होता है जब निम्न प्रकृति को वशीभूत न किया जाये। अविकसित अवस्था में आँखें बन्द कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। इससे किंचिन्मात्र भी लाभ नहीं होगा।
केवल पवित्र मन से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्राचीन मनीषियों ने बड़ी बुद्धिमानी से चार विधियों को प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम पूज्य भाव से निष्काम सेवा करके अपने स्वभाव को पवित्र करो। मन पवित्र होने पर एकाग्रस्थ होने का यत्न करो तथा विविध प्रकार की औपचारिक पूजा से मन को स्थिर करो। इसके उपरान्त ही आप गहन ध्यान द्वारा माया के आवरण का अवछेदन करके अलौकिक आनन्द प्राप्त कर सकेंगे। जब तक आप आत्म-चैतन्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक शुद्धि के लिए कर्मयोग, मन-संयम करने के लिए भक्तियोग एवं अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गहन चेतना में जाने के लिए राजयोग का अभ्यास करो। आत्म-साक्षात्कार तभी होता है। ज्ञानयोग साक्षात्कार ही है।
इन गुणों को सदा स्मरण रखना चाहिए- पवित्रता, निष्काम सेवा, निरहंकारिता, अर्थात् संयत एवं विरक्त जीवन। ध्यान में मन को एकाग्र करने के लिए विविध युक्तियाँ बतायी गयी हैं। हम देख चुके हैं कि प्राणायाम किस प्रकार द्विविध रूप में सहायक है। मन एवं श्वास अन्योन्याश्रित हैं। श्वास रोकने से मन वशीभूत हो जाता है। प्राण वशीभूत होने पर सत्त्व बढ़ता है। सत्त्व एकाग्रता में सदा सहायक होता है। रजस् एवं तमस् एकाग्रता में सहायक नहीं हैं। अतएव प्राणायाम से दो लाभ हैं-इससे शरीर को सात्त्विक बनाने एवं मन को स्व-लक्ष्य पर केन्द्रित करने में सहायता मिलती है।
यदि एकाग्रता के लिए एक ही विधि का अनुसरण किया जाये तो कभी-कभी उबाने वाला हो जाता है। अतएव, विविध विधियों द्वारा अभ्यास करते रहना चाहिए। सान्ध्य तारा, चाँद अथवा अन्तर्मन की आवाज पर ध्यान करने का यत्न करना चाहिए। किसी सुखकर रंग का भी ध्यान किया जा सकता है। आसन लगाने के उपरान्त उन रंगों की कल्पना करना भी हितकर है जिन्हें आप सबसे अधिक पसन्द करते हैं। कुछ व्यक्तियों को नीला रंग पसन्द है तो कुछ को लाल रंग अच्छा लगता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि है। रंग कोई भी हो, जो आपको सर्वाधिक पसन्द है-चुना जा सकता है। उसी में आपका अन्तःकरण रंग जाये। उसे दृढ़तापूर्वक बनाये रखें। कुछ लोग गुलाब की सुगन्ध पर मन एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा अनुभव करने का प्रयास कीजिए जैसे आप किसी सुरभि-सागर के मध्य में हों। इस प्रकार भी एकाग्रता हो सकती है अथवा इसके लिए किंचित् अन्य स्थूल एवं भौतिक पदार्थों को भी लिया जा सकता है। लोग दीपक जला कर उस पर या दीवार पर बिन्दु बना कर उस पर भी मन एकाग्र करने का यत्न करते हैं। कुछ व्यक्ति मन को अन्तर्मुख करके; परन्तु आँखें खुली रख कर भी ध्यान लगाते हैं। इसे शाम्भवी मुद्रा कहते हैं।
मन को विविध प्रकार की ध्यान-प्रणालियों यथा-सूक्ष्म ध्यान- प्रणाली से स्थूल ध्यान-प्रणाली, निराकार ध्यान-प्रणाली, बाह्य ध्यान से एकाग्र करने के लिए अभ्यास करना चाहिए।
कभी-कभी मन के साथ शिशु के समान व्यवहार करना पड़ता। कभी इसे कोई सुन्दर पदार्थ (विषय) का लालच देना पड़ता है और कभी वाग्दण्ड देना पड़ सकता है। अतः आवश्यकतानुसार समय-समय पर विविध युक्तियों से मन को एकाग्र किया जा सकता है। ये कतिपय विधियाँ हैं जिनके द्वारा मन को एकाग्र एवं अन्तर्मुख करके ध्यान में प्रवृत्त किया जा सकता है।
समाधि
अविरत अभ्यास एवं वैराग्य में सम्यक् अवस्थिति होने से एकाग्रता बढ़ती है तथा अखण्ड क्रम से चलती रहती है और अन्ततः गहरे ध्यान में निमग्न होने की अवस्था आती है जो राजयोग की आठवीं अवस्था है। इसे समाधि कहते हैं। परन्तु 'समाधि' शब्द उन शब्दों में से एक है जिसका अर्थ व्यापक रूप से अन्यथा ग्रहण किया जाता है। प्रश्न उठता है-समाधि क्या है? इस शब्द से सब परिचित हैं; परन्तु उचित अर्थ जानने वाले बहुत कम हैं। 'समाधि' के युक्तार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधक को कई तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है।
प्रथम, समाधि राजयोग की आठवीं अवस्था है। योग में समाधि केवल एक अवस्था ही है, सिद्धि नहीं। विशेषकर राजयोग में यही एक तथ्य है जिसका सम्यक् ज्ञान आवश्यक है। यदि कोई साधक समाधि लगा लेता है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वह सिद्ध योगी है, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है या साक्षात्कार कर लिया है। उसे अभी और आगे बढ़ना है। यह समाधि केवल राजयोग की ही विशेषता नहीं है। ज्ञानीजन अद्वैत निर्विकल्प समाधि की बात करते हैं। हठयोगियों ने प्राण एवं अपान का संयोग करके उन्हें सुषुम्ना द्वारा निकाल कर समाधि प्राप्त की है। इन प्राणों को पृथक् पृथक् मुद्राओं और क्रियाओं द्वारा सुषुम्ना नाड़ी एवं विभिन्न चक्रों में से लाया जाता है और तभी समाधि लग जाती है। भक्तजन इसे भाव समाधि में जाना कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजयोग की आठवीं अवस्था 'समाधि' हठयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग में भी पायी जाती है। इन पृथक् पृथक् समाधियों में अन्तर क्या है? नाम मात्र का ही अन्तर है अथवा वास्तव में भी कुछ अन्तर है? और इन सब समाधियों का क्या उद्देश्य है? क्या ये सब एक ही अर्थ में प्रयुक्त होती हैं अथवा भिन्न-भिन्न अर्थों में ?
राजयोग में चित्तवृत्ति के गहन एवं अविरत रूप से एकाग्र होने पर योगी ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें एकाग्रता द्वारा वह मन को पूर्णरूपेण संयत एवं शान्त करने के योग्य हो जाता है। इसी अवस्था को समाधि की अवस्था कहते हैं। यह अवस्था गहरी तन्मयता, तादात्म्य की अवस्था है। सम्यक् धारणा के उपरान्त मन की यह अन्तर्मुखी तन्मयता की अवस्था है। मन की भली-भाँति पकड़ इसी अवस्था में होती है। मन की यह पकड़-निरोध ही 'समाधि' कही जाती है। यह संस्कृत-व्युत्पन्न शब्द है। यह आवश्यक नहीं कि विलीनता की अवस्था अलौकिक आनन्द की अवस्था हो। कुछ समय की अवधि के उपरान्त भी दस, पन्दरह, बीस, तीस मिनट की सीमा तक जैसा योग की पुस्तकों में निर्दिष्ट होता है, यदि कोई योगी अविरत रूप से चित्तवृत्तियों को बाँधने में सफल हो गया है तो ऐसा कहा जा सकता है कि उसने समाध्यावस्था प्राप्त कर ली है। प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करते हुए मन का निग्रह करने का यत्न कीजिए। समाधिस्थ होने का प्रयास करते-करते आप एक दिन दिव्य ज्योति प्राप्त कर लेंगे जो ब्रह्मज्ञान को (आपमें) आलोकित करती है। इसके द्वारा आप चेतना की उच्चतम भूमिका तथा अलौकिक प्रकाश प्राप्त कर लेंगे जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजयोग में विविध प्रकार की समाध्यावस्थाओं का वर्णन है जिनका अभ्यास मोक्ष-प्राप्ति-पर्यन्त आवश्यक है।
ध्यानावस्था, जिसमें आप अत्यन्त लीन हैं; परन्तु आपको अपने व्यक्तित्व की सत्ता का आभास रहता है-यह एक प्रकार की समाधि है। उत्तरोत्तर बढ़ने पर आपके व्यक्तित्व का चैतन्य भी ब्रह्म-चैतन्य की प्रतीति में विलीन हो जाता है। यही आत्म-साक्षात्कार है। इसी अवस्था को राजयोगी समाधि कहता है। हठयोगियों की समाधि में मुद्राओं एवं प्राणायाम द्वारा मन में कुछ गुह्य जटिल अवस्थाएँ उत्पन्न की जाती हैं और मन सर्वथा तल्लीन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समाधि में वृत्तियाँ सर्वदा के लिए नष्ट नहीं होतीं। अतएव, इस समाधि में अलौकिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। यह तो केवल अवरोध की अवस्था है। यह पूर्ण अवरोध है। वृत्तियों का उन्मूलन इसमें नहीं होता। अतः परिणाम क्या होता है? सामान्य चेतना के लौटने पर ज्ञात होता है कि वृत्तियाँ ज्यों-की-त्यों विद्यमान हैं। वृत्तियाँ जिन्हें जड़ समाधि में प्रशमित किया गया था, पुनः कुछ सीमा तक क्रियाशील हो जाती हैं। अतएव, यह जड़ समाधि, जिसे विशेष हठयौगिक विधाओं जैसे-मुद्रा, प्राणायाम आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है, (जन्म-मरण के बन्धन से) मुक्त नहीं कर सकती, ऐसा कुछ लोगों का विचार है।
ज्ञानियों की समाधि न्यूनाधिक रूप में राजयोगियों की समाधि के समान है। राजयोगी सर्वव्यापक परम पुरुष पर ध्यान केन्द्रित करके समाधि प्राप्त करते हैं। ज्ञानयोगी अनाम, निराकार एवं सर्वव्यापक आत्मन् में ध्यान लगाता है और यह सर्वथा निर्विकल्प समाधि होती है। इसमें ध्याता के व्यक्तित्व का बोध लेश-मात्र भी नहीं होता। उसका व्यक्तित्व पूर्णतः निःशेष हो जाता है। आप जानते ही हैं कि ज्ञान के क्रम में सर्वप्रथम ज्ञाता, फिर ज्ञान का विषय एवं अन्ततः ज्ञान-प्रक्रिया होती है; परन्तु जब ज्ञाता ही नहीं रहता, तब क्या होता है? ज्ञाता के न होने पर ज्ञान के विषय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब एक ही तत्त्व शेष रह जाता है। शेष केवल अस्तित्व रहता है, वही सत्त्व है। इसे अद्वैत निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसमें ज्ञाता, ज्ञान-विषय एवं ज्ञान-ग्रहण करने की प्रक्रिया उस अनन्त, असीम, लोकोत्तर अनुभूति में लीन हो जाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्णन करने वाला ही नहीं होता। जब अनुभव-कर्ता ही अपनी सत्ता से ऊपर उठ गया है, तो अनुभव कौन करेगा ? एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को और स्पष्ट किया जाता है। आपके पास नमक से बनी हुई एक सुन्दर गुड़िया है। आप उसे सागर के तट पर ले जाते हैं। अकस्मात् ही उसमें इच्छा उत्पन्न होती है- "देखूँ तो सही यह सागर कैसा है, कितना गहरा है?" और वह सागर में डुबकी लगाती है। सागर में प्रवेश करते ही नमक घुल कर विलीन हो जाता है और वह सागर के साथ ऐक्य प्राप्त कर लेती है। अब केवल सागर का अस्तित्व ही शेष रह जाता है।
अतएव ज्ञानयोगी कहते हैं कि सर्वोच्च लोकोत्तर अनुभव ब्रह्म का बोध ही है। भक्तियोग में निर्विकल्प समाधि प्रभु-दर्शन होने पर ही लग सकती है। भक्त उपासक होता है और जब वह अपने आदर्श (इष्टदेव) के दर्शन कर लेता है, तब उसके व्यक्तित्व की विलीनता आरम्भ होती है। यह सब तत्काल नहीं हो जाता; किन्तु शनैः-शनैः भक्त का अस्तित्व विलय होने लगता है। अन्त में आदर्श ही शेष रह जाता है। मीरा अपने प्रभु के पास गयी और उसी में अन्तर्धान हो गयी। भक्तियोग के अनुसार इसे 'सायुज्य' कहते हैं। प्रभु के साथ एक होना सायुज्य है। पानी से भरा हुआ एक बरतन जिसमें सूर्य की रश्मियाँ प्रतिबिम्बित हो रही हैं, यदि तोड़ दिया जाये तो रश्मियाँ सूर्य में विलीन हो जायेंगी। इसी तरह दिव्य जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेने पर भक्त का व्यक्तित्व निःशेष रूप से ईश्वर में समा जाता है।
ईश्वर-सायुज्य के प्रति दार्शनिकों का दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार है। उदाहरणतया हिमालय पर्वत की भाँति ऊँचे एक चीनी के पर्वत पर यदि चीनी का एक कण और रख दिया जाये तो इसे पृथक् रूप से पहचानना असम्भव है। इसे पृथक् भी नहीं किया जा सकता। तथापि, वह अपना अस्तित्व तो रखता ही है।
यदि कोई भक्त, ज्ञानी अथवा ध्यानी समाधि की गहन अवस्था में एक बार भी आत्म-साक्षात्कार कर ले तो वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तदुपरान्त कोई दुःख, क्लेश अथवा कामना शेष नहीं रह जाती। वह अपने लक्ष्य की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है जहाँ अन्य कोई तृष्णा शेष नहीं रहती। काया का अस्तित्व बने रहने पर भी वह नित्य-मुक्त और अमर हो जाता है। चाहे वह जीवित हो एवं चलता-फिरता हो, उसने पूर्णता प्राप्त कर ली है और ब्रह्म-साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे व्यक्ति की समाधि टूटने पर भी उसे समाधि का अनुभव स्मरण रहता है।
मोक्ष
इस भौतिक लोक में सब-कुछ अस्थायी है, अतः कोई भी पदार्थ हो, वह स्थायी आनन्द प्रदान करने में असमर्थ है। आनन्दानुभूति निःशेष होते ही निराशा होने लगती है। इसीलिए विद्वान् कहते हैं, 'सर्वं दुःखं विवेकिनः'- 'विवेकशील व्यक्तियों के लिए यह संसार दुःखमय है।' इस लोक में परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तथापि, मनुष्य स्थायी सुख को प्राप्त करने में निरत है। अतः ऋषिगण भी उद्घोष करते हैं-"मनुष्यो ! जागो। हमारा सन्देश सुनो। हमने उस अमर तत्त्व की खोज कर ली है, जिसमें समा कर आप शाश्वत आनन्द का अनुभव करेंगे। उस अवस्था को प्राप्त करो जो हमने प्राप्त की है।" यह उपनिषदों की पुकार है।
प्रत्येक जीव का अन्तिम लक्ष्य परब्रह्म का साक्षात्कार है। योग का अर्थ है-सीमित तत्त्व का असीमित तत्त्व से ऐक्य-आत्मा का परमात्मा में समा जाना। जिस प्रकार वर्षा का पानी नदियों से होता हुआ उसी सागर में जा कर मिल जाता है जहाँ से इसका उद्भव हुआ था, उसी प्रकार जीव जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, अन्ततोगत्वा उसी में समा जाता है। एक बार ऐसा होने पर सब हृदयग्रन्थियाँ खुल जाती हैं। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाती। इसका अर्थ है-सब कष्टों का प्रशमन एवं असीम आनन्द तथा शान्ति की प्राप्ति। कोई कामना शेष नहीं रह जाती, कोई तृष्णा नहीं होती, सम्पूर्ण प्राचुर्य की अनुभूति होती है। यह योग की पराकाष्ठा है।
आत्म-निरोध और अविरल प्रयत्न से अन्ततः योग-सिद्धि प्राप्त होती है, जहाँ परम आनन्द की प्राप्ति होती है। वह आनन्द किस प्रकार का है? कहते हैं यदि आप सागर की मछली पकड़ कर एक छोटे बरतन में रखें तो वह उस बरतन से बाहर आने का यत्न करेगी-उस असीम मुक्तावस्था को प्राप्त करने के हेतु, जिसका स्वाद वह पहले ले चुकी है। यदि कोई व्यक्ति सहानुभूतिवश उसको ले जा कर सागर में छोड़ देता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होगी। जल में वह इच्छानुसार पुनः इतस्ततः तैरना आरम्भ कर देगी।
यह एक रुक्ष दृष्टान्त है। अपरिमित स्वतन्त्रता की अनुभूति तो परमात्मा से ऐक्य होने पर होती है; परन्तु उस परमानन्द का ईषज्ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसे कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता। ऋषि-मुनि पुनः पुनः कहते आये हैं-"आप क्षणिक सुख के पीछे क्यों भाग रहे हैं? विषय-भोग के अतिरिक्त आपको वास्तविक आनन्द का बोध ही नहीं है। इस विश्व में प्राप्त होने योग्य आनन्द की आपकी सर्वोच्च धारणा क्या है? आप उत्तर देंगे कि आपकी सब इच्छाएँ पूर्ण होनी चाहिए। यही महत्तम सुख है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं; परन्तु सभी कामनाएँ तो किसी की भी पूर्ण नहीं होर्ती!" इस संसार में जिसके पास सब पदार्थ हैं, केवल उसी को यह सुविधा प्राप्त है।
एक साधारण भौतिक जीव की क्षुधा भौतिक ही होगी। वह शारीरिक सुख में ही आनन्दित होता है। वह अनुभव कर सकता है कि उसकी त्वचा को क्या रुचिकर है। सौन्दर्य-शास्त्र का प्रेमी संगीत में आनन्द ले सकता है; परन्तु एक साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता। साधारण व्यक्ति संगीत के स्वाद से अनभिज्ञ है। वह एक अत्यन्त सुन्दर चित्र की भी प्रशंसा नहीं कर सकता; क्योंकि उसमें कलात्मक भाव की कमी है। सूर्योदय हो अथवा सूर्यास्त, उसके लिए सब समान है। इन्द्रियाँ भी जितनी ही परिष्कृत होंगी और सौन्दर्य-बोध जितनी मात्रा में उदय होगा, उतना ही विस्तृत सुख का क्षेत्र हमारे लिए प्रस्तुत होगा। सौन्दर्य के प्रति प्रेम होने पर आप उत्तम संगीत एवं सर्वोत्कृष्ट कला का आनन्द ले सकते हैं। सुख-प्राप्ति के हेतु जब आपको सब श्रेष्ठ युक्तियों की प्रतीति हो जाती है तब आप स्थूल इन्द्रिय-विषय-सुख की ओर नहीं भागते और रुग्ण नहीं होते। अतः कोई भी व्यक्ति वैभवशाली हो कर भी यदि आत्म-संयम रखे तो सब सांसारिक सुख भोग सकता है। वह काव्य, चित्रकला आदि का रसास्वाद ले सकता है और संसार-भर में सम्मान प्राप्त कर सकता है। वह इस बात को जान कर सन्तुष्ट रहेगा कि वह जगत् का स्वामी है। इस संसार में रहते हुए आपकी सुख की सर्वोच्च संकल्पना यही हो सकती है।
कहा जाता है कि यदि इस प्रकार के सुख की कल्पना सम्भव है और यदि कोई व्यक्ति यह सब प्राप्त कर भी लेता है, जैसे-हर प्रकार के विषय-सुख, सुस्वादु व्यंजन, उपभोग आदि तो इन सबका भोग करने वाले व्यक्ति के सब सुखों को यदि इकाई मान लिया जाये तो एक पुण्यात्मा मानव-गन्धर्व के सुख का परिमाण शत गुणा अधिक होगा। देव-गन्धर्वो का सुख, मानव-गन्धवों से सुख से शत गुणा अधिक कहा जाता है। पितरों का सुख, जिनका संसार नित्य है, देव-गन्धों से सुख से शत गुणा अधिक एवं इसी भाँति स्वर्ग में उत्पन्न देवताओं का सुख एवं कर्मदेवों का सुख क्रमशः पितरों एवं देवताओं के सुख से शत-शत गुणा अधिक माना जाता है चाहे वह परिमाण में हो अथवा प्रबलता में। स्वादिवों का सुख कर्मदेवों के सुख से शत गुणा अधिक है, उससे भी सौ गुणा अधिक सुख प्राप्त है इन्द्र को, जो स्वर्ग के देवताओं का स्वामी है। देवगुरु बृहस्पति को इन्द्र से भी शत गुणा अधिक सुख प्राप्त है। इसे यदि शत गुणा कर दिया जाये तो बिराद का एक सुख माना जाता है। विराट् को प्राप्त सुख से शत गुणा अधिक है ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता) का सुख, आनन्द; परन्तु इससे अनन्त गुणा अधिक सुख है परब्रह्म का।
विश्व-सम्राट्, मानव-निर्मित देवदूत, देवदूत से वास्तविक स्वर्गदूत और फिर पितर, कर्मदेव, वास्तविक देवता, इन्द्र, बृहस्पति, विराट्र, हिरण्यगर्भ एवं परब्रह्म-शास्त्रों में दिव्यानन्द का लेखा इस प्रकार है। अतः योगाभ्यास द्वारा प्राप्त सर्वशक्तिमान् परमात्मा का आनन्द अनिर्वचनीय है। अतएव, इसे दिव्योन्माद कहा जाता है। उसकी अभिव्यंजना नहीं हो सकती। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं समाधि द्वारा प्राप्त सर्वोत्कृष्ट फल है-ब्रह्म-चैतन्य। राजयोग की आठ अवस्थाओं के अभ्यास से योगी इसी ब्रह्म-साक्षात्कार-रूपी फल को प्राप्त करता है। यह अपार आनन्द की अवस्था होती है जिसमें व्यक्तिगत चेतना परम तत्त्व में विलीन हो जाती है। अनुभवकर्ता इसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। वह मूक-सा हो जाता है। यथा मूक प्राणी किसी स्वादिष्ट पदार्थ का स्वाद नहीं बता सकता, उसी प्रकार परमानन्द में लीन होने के पश्चात् योगी आनन्दमय हो जाता है; परन्तु उस परम आनन्द का वर्णन नहीं कर सकता। यह उच्चतम समाधि की अवस्था है। हम जब तक समाधि की उच्चतम अवस्था नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक इतना ही आनन्द प्राप्त कर सकते हैं।
अद्भुत बाद्य संगीत सुन कर यदि कोई व्यक्ति आपको उसका विवरण दे तो आप उस संगीत के माधुर्य का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, समुचित रूप से उसकी पूर्ण धारणा नहीं कर सकते, संगीत का आनन्द नहीं ले सकते। अतः समाधि से प्राप्त आनन्द की आप तब तक केवल कल्पना ही कर सकते हैं जब तक आप स्वयं उस आनन्द का अनुभव न करें। समाध्यावस्था को प्राप्त करने वाले सन्तजन अभी भी विद्यमान हैं, यद्यपि उनकी पहचान कठिन है। युक्तभाव वाला व्यक्ति ही इन महान् आत्माओं की पहचान करके उनसे पूर्णता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने उस अलौकिक रूप के दर्शन किये हैं, वे ही उस सौन्दर्य का वर्णन करने का यत्न करते हैं। संसार की सर्वाधिक सुन्दर नारियों के सौन्दर्य की उपमा यदि स्वर्ग की अप्सराओं से की जाये तो लौकिक स्त्री का सौन्दर्य उनके समक्ष नगण्य होगा। वे तो इतनी सुन्दर हैं कि मनुष्य उन पर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता; परन्तु आत्म-साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति को वह श्मशान भूमि की राख के समान दिखायी देंगी। उसके लिए वे जुगुप्सा की पात्र होंगी।
इस प्रकार हमने आत्म-साक्षात्कार के आनन्द का किंचित् ज्ञान प्राप्त किया। हमें सदा उसी आनन्द को प्राप्त करने का यत्न करते रहना चाहिए। इस आनन्द की तुलना में समस्त लौकिक विषयों से प्राप्त आनन्द भी नगण्य है। ब्रह्म-साक्षात्कार से प्राप्त आनन्द असीम है। उसकी कोई सीमा नहीं है। अनात्म का आनन्द सीमित आनन्द है। आत्मानन्द नित्य है। यह कभी नष्ट नहीं होता और आप यही आनन्द-स्वरूप हैं। यही आपका वास्तविक स्वरूप है; परन्तु अज्ञान एवं इच्छाओं के बन्धन में आ कर आप इसे भूल चुके हैं। इन्द्रियों को वश में करो, अज्ञान को दूर करो और अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। स्थिरता प्राप्त करो, परमात्मा को पहचानो और परमानन्द को प्राप्त करो। योग का यही सन्देश है।