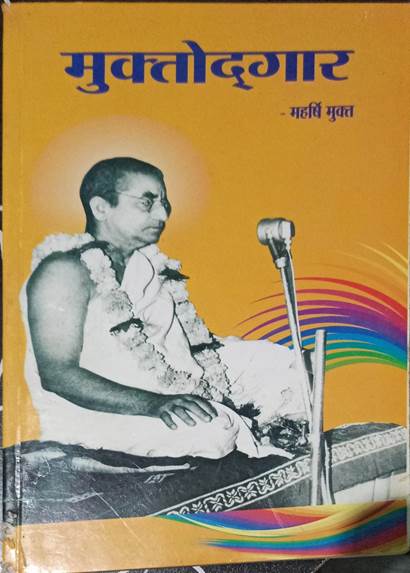
मुक्तोद्गार
जो दर्शन, प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा का
दर्शन करा दे, उसका ही नाम दर्शन है।
![]()
महर्षि मुक्त
मुक्तोद्गार
प्रकाशक :महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति
केन्द्र, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
(सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशकाधीन)
मुद्रक :नेचर ग्राफिक्स शांति चौक,
पुरानी बस्ती, रायपुर
मो.: 9302230478
संस्कृत :तृतीय, वर्ष : 2012
प्रति :1000
कार्यालय एवं - :डॉ. एस.एन. त्रिपाठी
पुस्तक मिलने 50/152, बंधवापारा, पुरानी बस्ती
का पता रायपुर (छ.ग.) - 492001
मो. : 9926130014
मूल्य
समर्पण
मातृदेवो भव ।
पितृदेवो भव ।
आचार्य देवो भव ।।
परम् पूज्य सद्गुरुदेव महर्षि मुक्त के
श्रीचरणों में सादर समर्पित
महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति
संक्षिप्त-कथन
'श्री महर्षि मुक्त' के उद्गार श्री महर्षि जी के परिचय के प्रतीक हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, निगम एवं स्वानुभूति प्रमाण संसिद्ध समस्त चराचर का अस्तित्व 'मैं' हूँ, 'मैं' हूँ इस प्रकार नित्य प्रस्फुटित सच्चिदानंद घनभूत भगवान आत्मा का साक्षात्कार कराना जिनके लिए हस्तामलकवत् है।
उपरोक्त अनादि, अक्षय सार्वभौम सिद्धान्त का सतत् प्रचार करना श्री महर्षि जी के जीवन का चरम लक्ष्य है।
अलं
परमानंद शास्त्री
रायपुर (छत्तीसगढ़)
तृतीयावृत्ति का प्रकाशकीय कथन
विगत कई वर्षों से 'मुक्तोद्गार' की मांग को देखते हुए इसके संकलनकर्त्ता श्री नरनारायण जी अवावाल से इस पुस्तक का पुनः प्रकाशन हेतु अनुमति प्राप्त कर, समिति इस नव कायाकल्पित, संशोधित मुक्तोद्वार की तृतीयावृत्ति जिज्ञासु पाठकों को भेंट करते हुए हर्षानुभव कर रही है।
वृद्ध योगी का किसी शैशव शरीर में परकाय प्रवेश करने के उपरांत भी उसके अनुभव में किंचित मात्र भी कमी नहीं होती। बस, इसी तरह मुक्तोद्वार का काया कल्पित नया रूप आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसमें उन सभी परिशिष्टों का समावेश ज्यों का त्यों किया गया है, जैसा कि इसकी प्रथमावृत्ति में है।
संशोधन में कहीं-कहीं पर त्रुटियाँ रह गयी हैं, इसके लिए समिति क्षमा चाहती है और पाठकों से अनुरोध करती है कि इसे सुधार कर पढ़ें।
महर्षि मुक्तानुभूति
साहित्य प्रचारक समिति
प्रस्तावना
'मुक्तोद्गार' में महर्षि मुक्त द्वारा समय-समय पर दिए गए प्रवचनों, वार्ताओं के माध्यम से अध्यात्म दर्शन का सार प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद भवतगीता के सूत्र 'स्वभावोऽध्यात्म' की एक विशद व्याख्या है यहां अध्यात्म का सार है स्व-भाव अर्थात् आत्म-भाव। प्रकटतः भाव दो ही होते हैं-आत्म-भाव और विषय-भाव। विषय-भाव को ही कभी 'अनात्म-भाव' भी कह दिया जाता है, किंतु, ऐसा वाक्-विपर्यय के फलस्वरूप होता है, न कि इसलिए कि अनात्म जैसा कोई वास्तविक अस्ति रूप होता है। अवश्य, विज्ञान अपने अध्ययन की सुविधा हेतु विषय-भाव को एकांतिक 'पदार्थ- भाव' का रूप दे देता है। किंतु उसका उद्देश्य भी अंततः 'पदार्थ' के स्व- भाव या आत्म-भाव को ही उजागर करना होता है। अब, जहाँ भी आटम- भाव है, वहाँ किसी न किसी तरह आत्मा का सन्निवेश अवश्य होगा। विज्ञान का 'पदार्थ' जड़ भाव है, इसलिए उसके आत्म-भाव का निदर्शन चैतन्य- धर्मी आत्मा के प्रकाश के बिना असंभव है। मूल प्रकृति में 'महत्' (विराट सृजनात्मक अवगमनात्मक बुद्धि) का स्फुटन बिना पुरुष (आत्मा) के सान्निध्य के संभव ही नहीं है। इस तरह आत्मा के सान्निध्य में अवगम्य पदार्थ (प्रकृति) ही अध्यात्म की दृष्टि में 'विषय' स्वरूपेण प्रस्तुत होता है। अर्थात् अध्यात्म-दर्शन में प्रकृति या पदार्थ का आत्म-भावी अस्ति-रूप अध्ययन की वस्तु बनता है, जबकि विज्ञान में वही विवक्त रूपेण (Abstraction) अनात्म के छद्म अस्ति-देश में प्रस्तुत होता है।
अब, यह एक विलक्षण सी बात है कि विज्ञान की शैली में पादार्थिक आत्म-भाव को अनात्म-भाव का वैकल्पिक रूप देकर प्रस्तुत किया जाता है। यह कैसे संभव होता है? इस तरह के जिन प्रश्नों या समस्याओं से विज्ञान की उद्भावना होती है उनमें अस्ति या सत् के स्वरूप के प्रति अज्ञानता या उसके ज्ञान के प्रति संदेह का दृष्टिकोण प्रधान होता है। इसके विपरीत, अध्यात्म में उक्त अज्ञानता या ज्ञान के प्रति संदेह न होकर उनके संदर्भ में जिज्ञासा का यह दृष्टिकोण होता है कि तद्-तद् रूपों में वे किस तरह सत् के अनिवार्यतः निदर्शित आत्म-रूप को विपर्यस्त कर देने में समर्थ होते हैं।
जूडो-क्रिश्चियन धार्मिक परंपरा में 'ईश्वर' की तरह विज्ञान में 'सत्' 'छुपा हुआ' होता है, जबकि भारतीय धार्मिक परंपरा और अध्यात्म में स्वयं-प्रकाश्य रूपेण प्रस्तुत रहता है। यह श्रीमत जिज्ञासा ही अध्यात्म की ही होते उत्सुकता और आश्चर्य की अभिव्यक्ति है। उसका जन्म अज्ञान या संदेह में अतः, जैसा कि महर्षि मुक्त कहते जिज्ञासा ही अध्यात्म की प्रवेशिका है, न कि प्रश्न या समस्याएँ। जिज्ञासा किसी अज्ञात उत्तर को ढूँढने की विधा न होकर, प्रस्तावित उत्तर के प्रति उत्सुकता और आश्चर्य की अभिव्यक्ति है । उसका जन्म अज्ञान या संदेह में न होकर ज्ञान में होता है, । अज्ञान या सन्देह-जन्य सत् के प्रकट ज्ञान-स्वरूप को समझाने के लिए होती है।
अध्यात्म और विज्ञान के बीच प्रकट अंतर को और अधिक स्पष्टतापूर्वक समझने के लिए हमें वेदांत के 'अध्यास' की धारणा पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि महर्षि मुक्त कहते हैं 'अध्यास' तीन तरह के होते हैं-देहाध्यास, जीवाध्यास और ब्रह्माध्यास। 'अध्यास' का अर्थ है- आत्म-भाव (सत्) पर अनात्म-भाव (असत्) का प्रक्षेप। यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक, यह कि चूँकि भाव मात्र ही सत् का अर्थ रखता है, जिज्ञासा होती है कि असत् या अनात्म भाव क्योंकर संभव हो पाता है और दूसरी यह कि चूँकि भाव के अर्थ में कभी अभावमूलकता नहीं होती, उसके संदर्भ में असत् का भासमान होना (प्रक्षेण रूपेण) कैसे संभव हो पाता है? जिन जिज्ञासाओं पर अध्यात्म की भूमि तैयार होती है, उन्हीं में उक्त दो जिज्ञासाएँ भी शामिल हैं।
कर्म जगत् में 'मैं' आत्म-भाव पर 'मेरा शरीर' के अध्यारोपण से 'देहाध्यास' होता है। यह तमोगुणजन्य है, अर्थात् अज्ञान-जन्य है। यहाँ 'मैं' आत्मा के लिए साधनवत् प्रस्तुत देह को आत्म-भाव से संश्लिष्ट समझ लेने का भ्रम छिपा हुआ है। उपासना (भावना) जगत् में 'मैं' आत्मा पर 'मेरा मन' का आत्मभावी अध्यारोपण होने से 'जीवाध्यास' होता है। यह रजोगुण जन्य है अर्थात् विषयमूलक संकल्प-विकल्प जन्य। 'मैं' आत्मा पर विषयावेष्ठित आवेग का आवरण होने से आत्म-भाव के 'विषयी' होने भ्रम के फलस्वरूप जीवाध्यास होता है। यह जैव-तृष्णा का क्षेत्र है। ज्ञान में जगत् में 'मैं' आत्मा पर आत्मेतर 'परमात्मा' के अध्यारोपण से 'ब्रह्माध्यास' होता है। यह सतोगुणजन्य है, अर्थात् दो क्षेत्रज्ञ-प्रभेद जन्य भ्रम (देह क्षेत्र और जीव-क्षेत्र में 'आत्मा' और मूल प्रकृति क्षेत्र में 'परमात्मा' के बीच भेव से पैदा हुआ भ्रम)। इन तीनों प्रकार के अध्यास या भ्रम का निराकरण इस सहज बोध से हो जाता है कि 'मैं' आत्मा पर ही देह-भाव, जीव-भाव व ब्रह्म-भाव आधारित है, जबकि स्वयं उस आत्म-देश में इन सभी भावों का अभाव हो वह सर्व का सर्व 'मैं' परम तत्व है, जिसमें एकांतिक आत्म-भाव की भावना का भी लोप हो जाता है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि वह परम-तत्व (आत्मा) किसी भी साधन-प्रवचन, श्रवण, निदिध्यासन, बुद्धि-द्वारा अप्राप्य है। वह अपनी ही प्रेरणा से, अपनी ही शक्ति से प्रकट होता है। यहीं भगवद्कृपा है।
अब, यद्यपि 'मैं' आत्मा सहज बोध गम्य है, सांसारिक मनुष्य में उसकी उद्भावना सरल नहीं है। सांसारिक मनुष्य 'इदम् गम्य' प्रपंच या विषय जगत् का जीव है, जबकि 'मैं' आत्मा का क्षेत्र 'अहंगम्य' है, स्वयं-प्रकाश्य है। प्रपंच क्षेत्र सदैव माना जाता है, जाना नहीं, जबकि 'मैं' सदैव जाना जाता है, माना नहीं। प्रपंच विकल्प रूपेण प्रस्तुत होता है, वह चित्त या मनोवृष्तिमूलक संकल्प में कारण भूत है, इसलिए उसमें संदेह या धोखा है, जो वस्तुतः सभी प्रकार के अध्यासों के मूल में हैं। दूसरी ओर, 'मैं' आत्मा का अहं प्रकाश्य क्षेत्र प्रपंच शून्य है, वह कभी विकल्प-रूपेण प्रस्तुत नहीं होता, उसकी प्रकाशता अबाधित व शाश्वत होती है। अतः मात्र आत्मा ही त्रिकालाबाधित सत् है। पुनः, चूँकि 'प्रपंच शून्यता' का अर्थ ही 'चित्त- वृत्ति निरोधता' है, सांसारिक मनुष्य द्वारा आत्मा या आत्म- क्षेत्र तक पहुँचने की पहली शर्त ही है चित्त-वृत्ति-निरोध अर्थात्, मनः संकल्पों की रोकथाम।
परंतु, चित्त-वृत्तियों या मनः संकल्पों का निरोध कैसे संभव है? शिक्षा द्वारा। और शिक्षा कैसे संभव है? गुरु द्वारा। मानव शिशु-काल से ही शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि देह-भाव, जीव-भाव जन्म से ही भासमान रहते हैं। प्रपंच में पड़ने के साथ ही तद्रूप में उसकी पहचान कर लेनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे जलाशय में पड़ने के साथ ही तैरना, जान लेना होगा अन्यथा डूबना ही होगा। इस दृष्टि से जैसा कि महर्षि मुक्त कहते हैं, शिक्षा चरित्र- निर्माण का उपक्रम है। फिर, चरित्र निर्माण के लिए अनुशासन आवश्यक है और अनुशासन के संयम-इंद्रिय-संयम के रूप में देह-भाव के क्षेत्र में संयम और संकल्प-संयम के रूप में जीव-भाव के क्षेत्र में संयमा इंद्रिय-संयम भोग-वृत्ति का संयम और संकल्प-संयम (नैतिकता या व्यवहार शलता) के गुणों वाली शिक्षा कभी प्रमुखतः धनार्जन के लिए नहीं होगी, जैसा कि पाश्चात्य प्रभाव में आज उसका स्वरूप है, वरन् वह होगी आत्म-बोध के लिए। आत्म-बोध ब्रह्मानुभव की भूमिका है। ब्रह्मानुभव के लक्ष्य की हष्टि से ही पारंपरिक भारतीय शिक्षा में बह्मचर्य का विधान है। किंतु, पुनः, चूँकि आत्मा और ब्रह्म, आत्म-बोध और ब्रह्मानुभव परस्पर भिन्न नही हैं, बह्य (आत्मा) ही साध्य है और साधन भी।
चित्त-वृतियों या मन के निरोध के उपाय को ठीक से समझने के लिए यह जानना चाहिए कि भाव मात्र ही मनोमय हैं। मन में ही सारा प्रपंच है, सभी भावों की उत्पत्ति और गति है। इस सर्वदा चंचल और सर्वथा मायावी मन के निरोध हेतु गीता में अभ्यास और वैराग्य का मार्ग सुझाया गया है। 'अभ्यास' का अर्थ है अ-मन हो रहने, चित्त-वृत्तियों में निर्लिप्तता का अभ्यासा चैतसिक विषयों को आत्म-भाव का प्रक्षेप मानकर उनका उपराम आत्मा में ही कर देना। अ-मन हो रहने से कर्म भी भाव-शून्य हो जाता है और इस तरह देह-भाव और जीव-भाव दोनों ही आत्म देश में लीन हो जाते हैं। 'वैराग्य' का अर्थ है, ब्रह्म के सत्-चित्-आनंद स्वरूप से अलग सभी अस्ति-भावों का त्याग । फलतः ब्रह्म (आत्मा) ही तत्त्वतः दृष्टव्य, श्रोतव्य, ज्ञातव्य, मंतव्य, जिज्ञासतव्य रह जाता है। पुनः, यह भी जानना चाहि कि यद्यपि अभ्यास और वैराग्य की चर्चा यहाँ साधन के रूप में की गई है. साध्य 'आत्मा' तक पहुँचकर वे भाव-स्वरूपेण नहीं ग्राह्य हो पाते। चूँकि 'मैं' आत्मा स्वरूपेण साध्य है, किसी साधन द्वारा नहीं, आत्मा तक पहुँचक अभ्यास और वैराग्य उसी साध्य में विलीन हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैन देह-भाव, जीव-भाव और ब्रह्म-भाव उनके आधार भाव 'मैं' आत्मा में विली होते हैं। आत्म भाववत्ता भूमा है, पूर्ण है, जबकि अन्य भावरूप अल्प है अपूर्ण हैं।
अब, यह देखना चाहिए कि यदि आत्मवत्ता ही आधारभूत आदि मानव स्वरूप है, तो इसे धारण करना ही उसके लिए परम श्रेयस्कर है, उसक परम 'धर्म' है। पुनः, चूँकि आधारभूत मानव-स्वरूप सर्वत्र और सर्वकाल एक है, मनुष्य की धर्म-धारणा भी सदैव एकरूप ही होनी चाहिए। आ पृथक-पृथक धर्मों की धारणा मात्र मान्यताएँ हैं, स्वरूप विक्षेप हैं, 'ह नहीं। मनोमय होने से वे राग-द्वेष मूलक भी होंगे। इसलिए ब्रह्मानुसंधान जो धर्म का मूल साध्य है, वे बाधक होंगे, प्रकाश के बदले अंधकार वाहिकायें। इतिहास में धर्मों के बीच संघर्ष के मूल में यही बात है। इसलिए वे कभी विश्व-धर्म की पात्रता नहीं रखते। विश्व-धर्म का आधार केवल सहज मानव स्वरुपवता या आत्मवत्ता है। इस दृष्टि से 'विश्व-धर्म' केवल मानव धर्म' के रूप में संभव है।
जैसा कि महर्षि मुक्त कहते हैं, मानव स्वरूपवत्ता का प्रथम प्रकाश्य तत्व है- आनंद । मनुष्य सहित सारा चेतन जगत् आनंद की खोज में निकली एक विराट जीवन-यात्रा है। मनुष्य आनंद के लिए ही सारी चेष्टाएँ करता है। ज्ञान, मंतव्य, जिज्ञासा सभी आनंद को लक्षित करते हैं। इंद्रिय, मन या बुद्धि के द्वारा बाह्य आनंद अल्प है, वह सुख (सु-ख) है, साधन-जन्य है और इसलिए अनिवार्यतः दुःख द्वारा परिसीमित है। इसलिए 'भूमा' ही वास्तविक आनंद का आश्रय है। वहीं इसीलिए ईश्वर है, सार्वभौम विश्व- धर्म है, भगवद् धर्म है। ब्रह्म को सत्-चित्, आनंद स्वरूप कहने का परिभाषिक अर्थ ही है-संदेह के अभाव में वह सत् है, अज्ञान के अभाव में वह चित् है, विरोध (वैराग्य) के अभाव में वह आनंद है, दूसरी ओर, अन्य भाव-क्षेत्र, 'मैं' आत्मा पर विवर्त का स्वरूप होने से संदेह, अज्ञान और विरोध से भरपूर है, इसलिए वहाँ सत्-चित्-आनंद की खोज सदैव एक मृगतृष्णा साबित होती है।
ऊपर मैंने महर्षि मुक्त के उद्गारों की कुछ मुख्य बातों को एक क्रम में रख कर समझाने का प्रयास किया है। निःसंदेह यह अत्यंत संक्षिप्त और नितांत अपर्याप्त है। उनके सारगर्भित वक्तव्यों की सही ग्राह्यता तो उन्हीं की लय में चलते हुए उनके विचारों का ग्रहण है। जो धैर्यपूर्वक ऐसा करेंगे वे निश्चय ही उनकी वैचारिक गहराई और साधनागत आध्यात्मिक लब्धियों में भागीदार बन सकेंगे।
इति !
(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय)
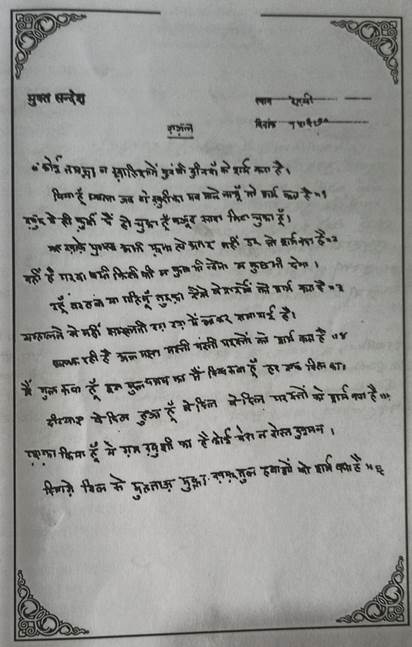
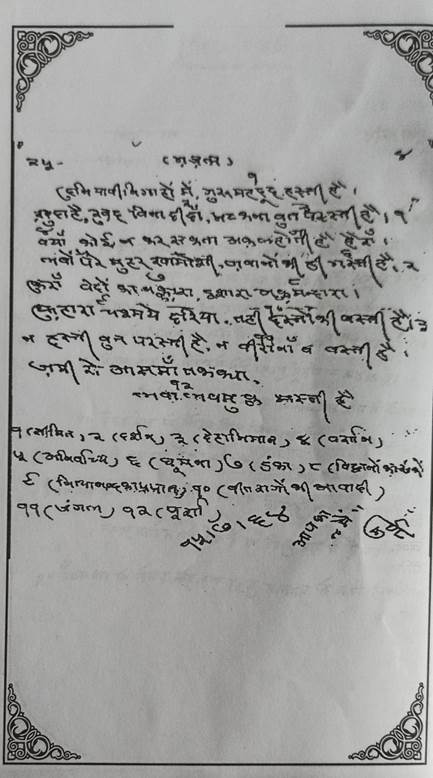
विषय-सूची
॥ श्री गणेशायनमः ।।
॥ श्री गुरुवे नमः ॥
卐 नारायणोपनिषद् 卐
ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्यधारिणी। नारायणाद् ब्रह्मा जायते। नारायणाद् रुद्रो जायते। नारायणाद् इन्द्रो जायते। नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते।
नारायणाद् द्वादशादित्याः सर्वे रुद्राः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। नारायणात् प्रवर्तन्ते। नारायणे प्रलीयन्ते।
अथ नित्यो नारायणः। ब्रह्मा नारायणः। शिवश्च नारायणः। शक्रश्च नारायणः। कालश्च नारायणः। दिशश्च नारायणः। विदिशश्च नारायणः। ऊर्ध्वं च नारायणः। अधश्च नारायणः। अन्तर्बहिश्च नारायणः।
नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति।
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!!
1.नाहं प्रकाश: सर्वस्य
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
मूठ्ठोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।।
(गीता 7/25
शब्दार्थ - भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि योगमाया से ढका हुआ में सबको प्रकाशित नहीं होता। अजन्मा अविनाशी मुझ आटमा को मूढ़ पुरुष नहीं जान पाते।
भावार्थ - अज्ञान से आच्छादित समस्त विश्व का 'मैं' सबको प्रकट नहीं हूँ, इसलिए जन्म-मरण रहित, सर्व के सर्व मुझ भगवान को अज्ञानी मनुष्य अनुभव नहीं कर सकते।
लक्ष्यार्थ- 'साक्षाद्परोक्षाद् ब्रह्म' इस श्रुति के कथनानुसार भगवान कहते हैं कि सम्पूर्ण चराचर के लिए 'मैं' अपरोक्ष हूँ अर्थात् किसी से छुपा नहीं हूँ, बल्कि प्रकट हूँ, परन्तु योगमाया का ढक्कन लगा हुआ है, इसलिए सब देख नहीं पाते। योगमाया कहते हैं नीचे ऊपर के ढक्कन को। जिस प्रकार
'मैं अरु मोरि तोरि तँ माया।' मैं-मेरा, तँ-तेरा ये दोनों नीचे ऊपर के ढक्कन हुए और 'मैं' आत्मा चेतन के संयोग हो जाने से नाम हो गया योगमाया। यानी मैं शरीर, मेरा शरीरा तैं शरीर, तेरा शरीरा यह कितना सुन्दर ढक्कन है! इसी के अन्दर 'मैं' आत्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान बन्द है और संसारी जीव भगवान के लिए अनादि काल से भटक रहा है। कहावट भी है-बगल में लड़का, शहर में ढिंढोरा।
आप भुलान्यो आप में बंध्यो आप ही आप ।
जाको ढूँढत फिरत है सो तू आपहि आप ॥
इसी प्रकार जीव अपने आपको साढ़े तीन हाथ का शरीर मानकर अविद्या की घोर निद्रा में सो रहा है। तभी तो गीताकार कहते हैं कि-
अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥
अर्थात् श्रद्धा, विश्वास से रहित पुरुष सर्व के सर्व 'मैं' आत्मा को न प्राप्त करके बार-बार जन्म-मरण के चक्र में पड़ता है और प्राप्त कौन करता है-
श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥
ज्ञान, साधन-चतुष्टय के अन्तर्गत सबसे मुख्य साधन 'श्रद्धा' है। श्री मानसकार भी कहते हैं कि -
भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ।।
(रामायण बाल.)
व्यवहारिक जगत् में भी श्रद्धा बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता तब भगवान का मिलना तो असम्भव ही है। इसलिए हृदय में श्रद्धा आ जाने से बाकी सब साधन अपने आप ही आ जाते हैं। श्रद्धा का वास्तविक अर्थ होता है गुरु और वेदान्त वाक्य पर अटूट विश्वास। पहला विश्वास तो गुरु (आचार्य) पर होना चाहिए और दूसरा श्रुति-स्मृति, सशास्त्र वेदान्त पर।
अब प्रश्न होता है कि गुरु के क्या लक्षण होते हैं? यूँ तो आजकल गुरुओं का बाजार लगा हुआ है। सभी गुरु अपने आपको ज्ञानी तथा सिद्ध होने का विज्ञापन करते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु का पहिचानना भी कोई सरल नहीं है, अपितु कठिन है।
विधि हरिहर कवि कोविद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी ।।
सो मो सन कहि जात न कैसे । साठा वणिक मणि गुण ठगन जैसे ॥
(रामायण बाल.)
जिन गुरुओं द्वारा आत्म कल्याण होता है उन गुरुओं का लाभ भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान और गुरु का अन्योन्याश्रय संबंध है। भगवान की कृपा से गुरु और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं और सत्य भी है, एक पहलू के दो नाम गुरु कहो अथवा भगवान। अब प्रश्न होता है कि भगवान की कृपा कब होती है और कैसे जाना जाय कि इसी गुरु के द्वारा मेरा आत्म कल्याण होगा? इसका समाधान यह है कि जिस समय हृदय में आत्म कल्याण के लिए मछली के समान तड़प पैदा हो जाय, यही भगवान की कृपा का स्वरूप है, जिसे कि वेदान्त शास्त्र में 'ब्रह्म जिज्ञासा' कहते हैं।
'अथातो ब्रहाजिज्ञासा ॥'
(ब्रह्म सूत्र 2/1)
सूत्रकार भगवान व्यास कहते हैं कि कुछ भी करना-धरना जब शेष नहीं रह जाता तब अन्त में आत्म कल्याण के लिए हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा पैदा होती है। उस समय कोई न कोई महान पुरुष प्राप्त हो जाता है और उसके वर्शन से अपने आप स्वभावतः चित्त का खिंचाव होता है, उसके पास बैठने पर चित्त कल्पनारहित हो जाता है एवं विलक्षण आनन्द का अनुभव होने लगता है। तब समझना चाहिए कि यही वास्तविक गुरु है और इसी के प्रसाद से मेरा आत्म कल्याण निःसंदेह होगा। परन्तु मन का खिंचाव तथा चित्त की निर्विकल्पता का अनुभव सात्विक हृदय को ही होगा, राजसी तामसी को नहीं। ऐसे गुरु के प्रति नारायण भाव होना अत्यावश्यक है, नर भाव नहीं।
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः ।।
(श्वेताश्व 6/23 )
अर्थात् जो पराभक्ति देव भगवान में होता है वही भाव आचार्य गुरु में भी हो तब उस महापुरुष का कथन किया हुआ आत्मा का उपदेश भली-भाँति आत्म जिज्ञासु के समझ में आता है, तभी आत्म कल्याण होता है। क्योंकि नर (जीव) से कल्याण नहीं होता, नारायाण द्वारा ही कल्याण होता है। जबकि जीव स्वयं अस्तित्वहीन है तब दूसरे का कल्याण क्या कर सकता है। भगवान गीताकार कहते हैं कि-
मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥
(गीता 7/3 )
अर्थात् हजारों मनुष्यों में कोई आत्म कल्याण के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में भी कोई तत्व से मुझको जानता है। इस श्लोक में सहस्त्रेषु शब्द आया है जिसका अर्थ हजारों यानी अनन्त होता है। सिद्धये का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए और तत्त्वतः का अर्थ होता है 'मैं' से। भाव यह है कि अनन्त मनुष्यों में कोई 'मैं ब्रह्म हूँ' इस ज्ञान सिद्धि के लिए यत्न यानी साधन करता है और साधनजन्य ज्ञान सिद्धों में भी कोई ही तत्त्वतः अर्थात् 'मैं हूँ' इस प्रकार से जानता है कहने का मतलब यह है कि 'अहं ब्रह्मास्मि' मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान साधनजन्य है। शास्त्र में इसको ब्रह्मानुसंधान (ब्रह्म की खोज) कहते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जानना भगवान को जानना नहीं कहा जा सकता। 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ इस साधनजन्य ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। इसी को ज्ञान दीपक कहते हैं। यथा -
सोहमस्मि इति वृति अखंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा ।।
(रामायण उ..)
क्योंकि, यह भी सतोगुण जन्य अध्यास है। 'मैं देह हूँ' यह देहाध्यास तमोगुण जन्य है। 'मैं जीव हूँ" यह जीवाध्यास रजोगुण जन्य है। 'मैं ब्रहा हूँ" यह ब्रह्माध्यास, सतोगुण जन्य है। इसलिए वस्तुतः भगवान को जानना यह है कि जिस 'मैं' देश में त्रिगुणात्मकजन्य तीनों भाव अथवा अध्यास इत्यादि सभी का अभाव है वह 'मैं' भगवान है। 'मैं देह हूँ' इस अध्यास का नाम कर्म जगत् है। 'मैं जीव हूँ' इस अध्यास का नाम उपासना जगत् है। 'में ब्रह्म हूँ इस अध्यास का नाम ज्ञान जगत् है।
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आटमवान् ।।
(गीता 2/45 )
अर्जुन तुम अर्थात् 'मैं' तीनों गुणों से परे निर्द्वन्द्व, नित्य, सत्वस्थ निर्योग एवं आत्मवान हो। क्योंकि, तीनों अध्यास 'मैं' के बिना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। 'मैं' सबको सिद्ध करता है, 'मैं' को कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। श्रुति कहती है कि 'दृष्टेद्रष्टारं न पश्येत्' अर्थात् दृष्टि के द्रष्टा को दृष्टि नहीं देख सकती।
येन सर्वं विजानीयात् तत्केन क विजानीयात् ।।
(वृहद, उप.)
भाव यह है कि जो सर्व का ज्ञाता है, उसका जालने वाला दूसरा कोई नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि- 'कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।' अर्थात् अनेकों ज्ञानियों में से कोई ही तत्व से जानता है। तत्व से जानने का मतलब यह है कि मैं को कुछ भी न मानकर मैं को 'मैं' ही जानना, यही तत्व से भगवान को जानना है। मानने और जानने दोनों के भाव भिन्न-भिन्न होते हैं। जो मानता है, उसको मन कहते हैं और जो जानता है उसको 'मैं' (आत्मा) कहते हैं। मानना मन का धर्म है, जानना आत्मा का धर्म है। जहाँ तक कुछ भी माना जाय वहाँ तक मन है। यानी मैं बहा हूँ यहाँ तक मन है, परन्तु जो बहा को भी जानता है, उसका नाम 'मैं' है और वही में 'मैं' हूँ। इस प्रकार के जानने को ही तत्व से जानना कहते हैं। इसी का नाम सहजपद, कैवल्यपद, सहजावस्था, सहजानन्द, सहज सनेह तथा भगवान की भरित है।
राम भगति चिंतामणि सुंदर । बसै गरुड़ जाके उर अंतर ।
परम प्रकाश रूप दिन राती । नहिं कछु चहिय दिया घृत बाती ।
पावन पर्वत वेव पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना ।
मरमी सज्जन सुमति कुवारी । ज्ञान विराग नयन उरगारी ।
भाव सहित जो खोजै प्रानी । पावै भगति मणि सब सुख खानी ।
सो स्वतंत्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ।।
परन्तु -
भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी । बिन सत्संग न पावहिं प्रानी ।
भगति तात अनुपम सुख मूला । मिलहि जो संत होहिं अनुकूला ||
संत विशुद्ध मिलहिं परतेहीं । चितवहिं राम कृपा कर जेही ॥
बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई ॥
(रामायण 3.)
फिर भी विचार वाटिका में परिभ्रमण कीजिए।
जे ज्ञान मान बिमत तव भव हरिणि भगति न आवरी ।
ते पाइ सुर दुर्लभ पदावपि पतत हम देखत हरी ।।
(रामायण उ.)
भाव यह है कि- हे प्रभो! जो ज्ञान के मान में उन्मत्त होकर तुम्हारी भव हरणि भक्ति का आदर नहीं करते, उनको दुर्लभ ज्ञान पद यानी अहं ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हूँ इस पद को प्राप्त करके भी इस पद से गिरते हम देखते हैं। क्योंकि अहं ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हूँ यह वृत्ति ज्ञान है और जहाँ पर इस अध्यसित ब्रह्म भाव का भी अभाव हो जाय 'मैं' ही रह जाय, सोई भगवान की भव हरणि भक्ति है अथवा कृतकृत्य पद है, परन्तु यह पद साधन जन्य नहीं, बल्कि कृपा जन्य है।
दुर्लभो विषयात्याको दुर्लभं तत्त्व दर्शनम् ।
दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां बिना ।।
(महोप, 4/77)
अर्थात् तब तक विषयों का त्याग तुर्लभ, तत्व का दर्शन, सहजावस्था इस भाव में उन्मत्तता एवं प्रमाव होना सम्भव है। क्योंकि, मैं बहा हूँ, यह दुर्लभ है जब तक कि सद्गुरु की कृपा न हो। मैं बहा हूँ (अहं ब्रह्मास्मि) साधन जन्य भाव है और साधन का फल सदैव अनित्य होता है, इसलिए इसमें अभिमान एवं प्रगाव होना स्वाभाविक है। क्योंकि, जिसका उत्थान है उसका पतन भी अवश्य है। जिस प्रकार जीव भाव में पतन था अर्थात् अपने आपको जीव मानकर कर्ता-भोक्ता, सुखी-दुःखी, नरकी-स्वी, ठगमनागमन इत्यादि मानता है, यही पतन का स्वरूप है और महान पुरुषों के सत्संग तथा सशास्त्र के विचार द्वारा उत्थान स्वरूप अहं ब्रह्मास्मि इस पद का बोध होता है कि मैं सत्, चित्, आनन्द, अखण्ड, अनन्त, अजन्मा, अजर, अमर, अद्वैत, सत्य, सनातन, व्यापक बहा हूँ। परन्तु यह भाव सत्संग एवं सशास्त्र अथवा सामवेदोक्त महावाक्य से तत्वमसि 'मैं' में लाया गया, किन्तु कालान्तर में कभी जा भी सकता है। परन्तु, जिस 'मैं' पर देह भाव, जीव भाव, ब्रह्म भाव इत्यादि सभी भाव आधारित है अथवा यूँ कहो कि जिस देश में समस्त भावों का अभाव है, वही अनिर्वचनीय पद, वास्तविक तत्व, सर्व का सर्व 'मैं' हूँ। यथा -
विशेष दर्शनि आटम भाव भावना विनिवृत्तिः ।
(योग दर्शन सू, कैवल्यपाद)
महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्वरूप का पूर्ण बोध हो जाने पर आत्मभाव की भावना की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जो जानना है यही तत्व से भगवान को जानना है। यह पद इतना सरल है कि इसकी सरलता ही कठिनाई है। यहाँ पर कुछ श्रुतियाँ आयी हैं, इनको भी सुनो - -
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥
भाव यह है कि आत्मा प्रवचन द्वारा, बुद्धि द्वारा, श्रवण द्वारा प्राप्त नहीं । जिज्ञासु का हृदय जब आत्म दर्शन के लिए मछली के समान तड़पताहै अथवा व्याकुल होता है तब तत्काल ही भगवान आत्मा सर्व का 'मैं' अपना स्वरूप प्रगट कर देता है। और भी सुनो -
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात् ।
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आटमा विशते ब्रह्मधाम ।।
(मु.उ 3 / 2 / 4)
भाव यह है कि बलहीन पुरुष को आत्मानुभव कभी नहीं होता। बल शब्द से यहाँ जिज्ञासा बल समझना चाहिए। आटम जिज्ञासा को ही आत्म कृपा भी कहते हैं, क्योंकि किसी और ने बांधा हो तो कोई खोले जबकि अपने संकल्प से स्वयं ही बंधा है तब अपने आप ही छूट भी सकता है।
अर्थ अविद्यमान जानिय संसृति नहिं जाय गोसाईं ।
बिन बांधे निज हठ शठ परवश परयो कीर की नाईं ॥
(विनयपत्रिका पद 20)
जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग् विधान् ।
(गौडपदीय का.)
अर्थात् साक्षात् परमात्मा ही अपने आप में सबसे प्रथम जीव भाव की कल्पना करता है कि मैं संसारी जीव हूँ, क्योंकि जीव की कल्पना का कोई आधार भी तो हो। तो विचार करने पर 'मैं' के अतिरिक्त दूसरा कौन होगा? बस, जीव भाव आते ही सारा प्रपंच भासने लग जाता है। जीव भाव के अभाव में जगत् का अभाव है और जीव भाव के भाव में अनन्त भावों का भाव है यदि महान शत्रु है तो जीव भाव।
सो माया बस भयऊ गोसाईं। बंध्यो कीर मरकट की नाई ।।
इसलिए अपने आप पर अपनी कृपा होना अत्यन्त आवश्यक है। गीताकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि -
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।।
(गीता 6/5)
अर्थात् अपने आपका उद्धार अपने आप ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हाँ, आचार्य गुरुजन लोग आत्म तत्व का उपदेश करते हैं, चेतावनी देते रहते हैं कि तू भगवान आत्मा है। स्थूल, सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से परे, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी, सत्, चित्, आनन्द, परिपूर्ण, अजन्मा, अजर, अमर समस्त चराचर का 'मैं', परात्पर सर्व का सर्व, सर्व के लिए अपरोक्ष आत्मा है। तीनों काल, तीनों अवस्थाओं में एक रस रहने के कारण तू सत् है। तीनों काल, तीनों अवस्थाओं के प्रपंच को जानने के कारण तू चित् है और तीनों काल, तीनों अवस्थाओं में सर्व को प्रिय है इसलिए तू आनन्द है।
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणः क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः ।
(श्वेता व. उप. 1/11 )
अर्थात् जिस देव को जानकर अष्टपाश, पंचक्लेश से जीव छुटकारा पा जाता है, सो देव तू है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश ये पंच क्लेश हैं और घृणा, शंका, भय, लञ्जा, निंदा, कुल, शील तथा जाति जीव के ये अष्टपाश हैं। असत् को सत्, चेतन को जड़, दुःख को सुख यानी साढ़े तीन हाथ के शरीर को आत्मा मानना, यही अविद्या है। द्रष्टा और दृश्य के धर्मों को एक जानना, यही अस्मिता है। इष्ट पदार्थ और वह जिसके द्वारा प्राप्त हो, दोनों के प्रति जो आसक्ति है यही राग है और दोनों के प्रति जो घृणा है यही द्वेष है। अनादिकालीन परम्परा से जिस मृत्यु के प्रवाह से बड़े-बड़े विद्वान भी डरते हैं यही अभिनिवेश है। पंचक्लेश एवं अष्टपाश से वही छुटकारा पा सकता है, जिसने अपने आप भगवान आत्मा को पहिचाना है।
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्त मानवाः ।
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥
(श्वेताश्व. उप 6/20)
अर्थात् आकाश को मृगचर्म के समान यदि कोई लपेट लेवे तब भी आत्मदेव को जाने बिना दुःख का अन्त हो जायेगा, ऐसा असम्भव है। अविद्या के चक्कर में पड़कर स्वयं परमात्मा होते हुए भी अपने आपसे भगवान को भिन्न मानता है। जब तक आत्मा-परमात्मा का भेद है, तभी तक माया का स्तित्व है।
यदा परात्मात्मविभेदभेदकं विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम् ।
तदैव माया प्रविलीयतेऽञ्जया सकारका कारणमात्मसंसृतेः ॥
(अ. रामायण रामगीता 18)
अर्थात् हृदयाकाश मंडल में प्रचंड सूर्य के समान विज्ञान का प्रकाश हो जाने पर आत्मा-परमात्मा का भेद मिट जाता है। तब तत्काल ही बंध्या पुत्र के समान अपने अधिष्ठान कारण सत्य सनातन ब्रा में हमेशा के लिए जीव आवागमन का कारण त्रिगुणात्मक विकारों के सहित माया लीन हो जाती है। यथा
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।
(गीता 7/14 )
गीताकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन। मुझ देव की यह त्रिगुणात्मिका माया दुरत्यया है अर्थात् इसका पार कोई नहीं पा सकता। हाँ, मुझको ही यानी 'मैं' आत्मा को ही जो जान लेते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। मतलब यह है कि अधिष्ठान को बिना जाने अधिष्ठान में कल्पित वस्तु का बोध नहीं होता। अपने स्वरूप 'मैं' (आत्मा) में माया उसी प्रकार है जैसे रज्जू में सर्प, ढूँठ में पिशाच, सीपी में चांदी तथा मृगतृष्णा में जला
माया, मन, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप ।
तब लग ये साँचौ लगें, नहिं जाना निजरूप ।
माया, मन, प्रकृति, जगत ये चारों पर्याय हैं और एक ही भाव के वाचक हैं।
रजत सीप महँ भास जिमि यथा भानु कर वारि ।
जदपि मृषा तिहूँ काल मंह भ्रम न सकइ कोउ टारि ।।
एहि विधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई ॥
झूठउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें ।
जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे यथा सपन भ्रम जाई ।।
( रामायण बाल. शंकरगीता-
इसलिए माया से पार होने के लिए अपने 'मैं' को भगवान जानकर अनुभव कर लेने पर ही माया से छुटकारा मिलता है, यानी संसार से तर जाता है। अपने 'मैं' को भगवान से भिन्न मानने पर ही जीव भाव है और जब तक जीव भाव है तभी तक संसार का बंधन अथवा गमनागमन का चक्कर है। यथा-श्रुति कहती है-
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रहाचके ।
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मटवा जुष्ट स्वतस्ते नामृतत्वमेति
(श्वे.3.1/8)
अर्थात सर्व के प्रेरक भगवान को अपने आपसे भिन्न मानकर अनादिकाल से हंस जीव ब्रह्म चक यानी संसार में भ्रमता रहता है और जब भगवान एवं अपने आप 'मैं' को शरीर से भिन्न करके एकता का अनुभव करता है, टाब यह तत्काल ही समस्त बन्धनों से सुफ होकर अमृत छ पद (कैवल्यपद) यह तलको जाता है। तात्पर्य यह है कि जितनी उपाधि है माया के ढक्कन ? को सायकल उठाते ही केवल 'मैं' का 'मैं' ही रह जाता है। श्रुति के इस कथन से यही सिद्ध होता है कि जीव का आवागमन इत्यादि भगवान से अपने आप 'मैं' को अलग मानने में ही है। इसलिए -
आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः ।
अविक्रियः स्वहम् हेतुर्व्यापकोऽसंग्यनावृतः ॥
एतैर्द्वादशभिर्विद्वानाटमनो लक्षणैः परैः ।
अहं ममेत्यसद्भावं देहादौमोहजं त्यजेत् ॥
(श्रीमद्भागवत् 7/7 / 19, 20 )
अर्थात् विचारवान पुरुष को चाहिए कि अपने स्वरूप आत्मा के बारह लक्षणों को भली-भाँति जानकर देहादिकों में जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ मैं, मेरापन है, इस भाव का त्याग कर मुक्त हो जाय। अपने आप 'मैं' के बारह लक्षण कौन से हैं? विचार कीजिए-मैं नित्य हूँ मैं अव्यय अर्थात् पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ यानी देहादिक प्रपंच का ज्ञाता हूँ, मैं सर्व का आश्रय (आधार) रहित हूँ, 'मैं' अकर्त्ता हूँ, मैं अपने आप स्वयं द्रष्टा हूँ, मैं सर्व का कारण हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं असंग हूँ (निर्लेप हूँ) मैं आवरण (अज्ञान) रहित हूँ, इन्हीं बारह लक्षणों को अपने स्वरूप आत्मा ('मैं') में जानकर सुमेरु पर्वत के समान अचल हो जाना चाहिए। अब प्रश्न यह होता है कि अपने आप 'मैं' को किस प्रकार और कौन-सी युक्ति के द्वारा शरीर से अलग करना चाहिए। समाधान यह है कि यथा -
स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् ।
क्षेत्रेषु देहेषु तथाऽऽत्मयोगै रध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत् ॥
अर्थात् हेमकार यानी सोनार, सोने को गलाकर खोट भाग को त्यागकर स्वर्ण का खरा भाग ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जहाँ तक मेरा कहा जाता है अथवा जिस पदार्थ के लिए मेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह सब खोट है और व्याज्य है। शेष जो 'मैं' रह जाता है, वहीं स्वर्ण के समान खरा अपना आप 'मैं' नाम से प्रसिद्ध भगवान आत्मा सर्व का सर्व है। क्योंकि 'मैं' में कोई धोखा नहीं, बाकी सब में धोखा है, इसलिए उपनिषद् की भाषा में श्रुति 'मैं' आत्मा को प्रत्ययसार कहती है। प्रत्यय-सार का अर्थ होता है विश्वासपात्र। व्यवहारिक जगत् में भी कोई व्यक्ति किसी अपने से उच्च पद पर आसीन महानुभाव के लिए जब कभी आवेदन-पत्र लिखता है, तो लिखता है कि 'आपका विश्वासपात्र (अमुक)।' यह विचारणीय विषय है कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुष्टय अन्तःकरण, प्राण, अपान, समान, ब्यान, उदान, पंच प्राण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय पंच कोश, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि क्या ये कभी विश्वासपात्र हो सकते हैं, जबकि ये सभी असत्, जड़, दुःख रूप, मिथ्या, उत्पत्ति विनाशशील एवं परिवर्तनस्वरूप हैं तो फिर विश्वासपात्र कौन हुआ, 'मैं' अथवा ये सब प्रपंच ? जबकि सारा प्रपंच असत् और मिथ्या है तब यह विश्वासपात्र कैसे हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि ये शरीरादिक असत् और मिथ्या कैसे हैं अथवा असत् तथा मिथ्या का लक्षण क्या है? असत् कहते हैं जो तीन काल में न हो और मिथ्या कहते हैं जो उत्पन्न होकर नाश हो जाय। शरीर बंध्यापुत्र के समान असत् है और पैदा होकर नाश हो जाता है, इसलिए मिथ्या है। यहाँ शंका होती है कि शरीर को या तो असत् कहो या मिथ्या कहो, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। समाधान यह है कि आत्म देश में शरीर असत् है यानी बंध्यापुत्रवत् है। जिस प्रकार बंध्यापुत्र अनुत्पत्ति रूप है उसी प्रकार प्रपंच अनुत्पत्ति रूप है, इसलिए असत् है और शरीर देश में शरीर उत्पन्न होकर नाश हो जाता है, इसलिए मिथ्या है। जिस प्रकार सूर्य देश में अंधकार नहीं, इसी प्रकार 'मैं' देश में ब्रह्मा से आदि तृण पर्यन्त समस्त प्रपंच नहीं। इसी पर श्री मानसकार जी कहते भी है कि -
रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानुकर बारि ।
यदपि मृषा तिहुँ काल मंह भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥
(रा.बा. दोहा 117)
यहाँ पर जगत् प्रपंच को मिथ्या कहा। फिर कहते हैं कि -
एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई ।।
(रा.बा. शंकर गीता)
यहाँ पर जगत को असत् कहा है इसलिए शरीर असत् भी है और मिथ्या भी है। अब प्रश्न होता है कि शरीर पैदा होने के प्रथम क्या था, भाव रूप था अथवा अभाव रूप था यानी सत् था या असत् था। यदि कहो कि उत्पन्न होने के पूर्व सत् था तो सत् की तो उत्पत्ति ही नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति मानने पर नाश भी मानना पड़ेगा और सत् कहते हैं जो त्रिकालाबाध्य हो, यानी उत्पत्ति विनाश से रहित हो। इसलिए सत् मानकर भी शरीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। अच्छा, यदि कहो कि शरीर उत्पत्ति के पूर्व असत् था तो असत् मानकर भी शरीर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, क्योकि जो तीन काल में न हो, बंध्यापुत्र के समान हो, उसे असत् कहते हैं। यानी जो है ही नहीं वह पैदा क्या होगा। अब यदि कहो कि शरीर पैदा होने के पूर्व सत्-असत् दोनों था, तब भी नहीं बनता, क्योंकि एक अवस्था में साधक-बाधक पदार्थ कदापि नहीं रह सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार से शरीरादिक प्रपंच की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। अब यदि कहो कि यह जगत् प्रपंच भगवान ने पैदा किया तो भी नहीं बनता, क्योंकि प्रश्न यह उठता है कि जिस भगवान ने प्रपंच पैदा किया वह भगवान जन्मा है अथवा अजन्मा है। यदि भगवान को जन्म वाला मानो तो भगवान नहीं, क्योंकि जन्म लेने वाला नाशवान होता है और अजन्मा मानो तो उससे किसी का जन्म सिद्ध नहीं होता। इसलिए किसी भी तरह से 'मैं' आत्मा के अतिरिक्त किसी का भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए शरीर आत्म देश में असत् है और यदि मानते हो कि शरीर है, क्योकि यह प्रपंच भासमान है इसलिए मानना ही पड़ेगा कि शरीर है, तो यह कोई बात नहीं। न होते हुए भी बहुत सी चीजें भासती हैं। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार आकाश में नीलिमा । यद्यपि आकाश में नीलिमा तीन काल में नहीं है, परन्तु प्रत्यक्ष भास रही है। हाँ! नीलिमा देश में नीलिमा है। उसी प्रकार नीलिमा के समान 'मैं' आत्म देश में शरीर नहीं है। शरीर देश में शरीर है। इसलिए 'मैं' के जानने पर शरीर असत् है और शरीर मानने पर शरीर मिथ्या है। क्योकि प्रपंच मानने की चीज है और 'मैं' आत्मा जानने की चीज है। तात्पर्य यह है कि किसी भी देश, काल, वस्तु को जानने के लिए चलोगे तो जानने वाले के सिवाय और कोई भी चीज न मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ढूँठ में पिशाच भासता है, रज्जु देश में अंधकार के कारण सर्प भासता है, मरुस्थल देश में जल असत् होते हुए भी समुद्र उमड़ता हुआ प्रतीत होता है। परन्तु, एक बात और है कि जो असत् होकर भासता है वह स्वदेश यानी अपने देश में भासता है, विचार करने पर आधार में नहीं भासता। मतलब यह है कि सर्प अपने ही देश में प्रतीत होता है, रज्जू देश में नहीं। इसलिए शरीरादिक प्रपंच असत् तथा मिथ्या होने के कारण विश्वासपात्र कभी नहीं हो सकते। यदि विश्वास करने योग्य कोई पदार्थ है तो 'मैं' आत्मा ही हूँ, शेष सब में धोखा है। जानने की चीज 'मैं' है, बाकी सब मानने की। अभाव को माना जाता है। भाव को जाना जाता है। माना हुआ पदार्थ अस्तित्वहीन होता है, जाना हुआ तो अस्तित्व ही है। जिस प्रकार प्रकाश से ही प्रकाश का ज्ञान होता है, प्रकाश के अतिरिक्त और किसी से भी नहीं, इसी प्रकार 'मैं' से ही 'मैं' का ज्ञान होता है, दूसरे से नहीं। इसलिए 'मैं' आत्मा ही विश्वासपात्र हूँ। और कहाँ तक कहा जाय, विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो 'मैं' के बिना सिद्ध हो जाय। यहाँ तक कि परमात्मा भी 'मैं' से भिन्न हो जाने पर केवल कल्पना मात्र का ही विषय रह जाता है और वह भी अस्तित्वहीन हो जाता है, इसलिए 'मैं' ही विश्वासपात्र हूँ।
यदि कोई ईश्वर के संबंध में प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर है अथवा ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण है? तो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ही प्रमाण होगा, अन्य नहीं, उसी प्रकार जैसे प्रकाश को प्रकाश ही सिद्ध कर सरकता है अन्य नहीं। पुनः ईश्वर अहंगम्य है, इदम्गम्य नहीं। यदि ईश्वर को इदम् यानी 'यह ईश्वर है' इस भाव से माना जायेगा तो अनित्य एवं नाशवान होगा, क्योकि सारा प्रपंच इदम्गम्य होने के कारण असत्, जड़, दुःखरूप अथवा परिवर्तनशील है। इसलिए ईश्वर इदम् गम्य न होकर अहंगम्य है अर्थात् 'मैं' ही हूँ जिसका नाम ईश्वर, परमात्मा, भगवान अथवा कुछ भी कहो 'मैं' के ही पर्याय हैं। मैं को मैं ही देखता हूँ। मैं को मैं ही जानता हूँ। मैं का अनुभव मैं ही करता हूँ। मैं को माने या न माने, जाने या न जाने, देखें या न देखें, अनुभव करें या न करें। हर हालत में, हर काल में, हर अवस्था में, 'मैं' के सिवाय विश्वासपात्र दूसरा कौन हो सकता है।
अहं शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः ।
स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥
(शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति 31)
अर्थात् जो 'मैं' शब्द करके विख्यात यानी प्रसिद्ध है और एक ही रूप से सर्व में स्थित है वह स्थूल अनेक रूप वाला शरीर कैसे हो सकता है। तभी तो श्री मानसकार जी कहते हैं कि -
ज्ञान अखण्ड एक सीतावर । माया वस्य जीव सचराचर ॥
(रामायण उ.)
अर्थात् जिसका ज्ञान अखण्ड है और एक है, वही सीतावर है। कितना विलक्षण भाव है। अर्थात् जो जागत के प्रपंच को जानता है वही स्वप्न को जानता है, जो जाग्रत और स्वप्न को जानता है वही सुषुप्ति के आनन्द का अनुभव करता है। जो तीनों अवस्थाओं को जानता है, वही तीनों काल को जानता है। कौन सा देश, कौन सा काल, कौन सी वस्तु है कि जिसको में आत्मा सर्वस्थान से सर्व को न जानूँ। इसलिए मैं ही विश्वास पात्र सर्व का सर्व साक्षात् भगवान आत्मा हूँ। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि - -
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।।
(भ.गो.अ. 7 श्लोक 25)
ॐ पूर्णमदः शान्तिः !!
2.चंचलं हि मनः
अर्जुन उवाच-
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।।
श्री भगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निवग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।।
(गीता 6/34/35)
अर्जुन का प्रश्न है कि भगवन्! आपने जो योग का उपदेश किया तथा आत्म चिंतन बतलाया सो ठीक है, परन्तु यह मन इतना चंचल, उन्मत्त एवं बलवान और वायु से भी अधिक वेग वाला है कि ऐसे मन का निरोध करना अत्यंत दुष्कर है अर्थात् असंभव-सा है। इस प्रश्न के उत्तर में श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि- 'तुम्हारा कहना यथार्थ है। यह मन निःसंदेह दुर्निग्रह है यानी इसका निरोध कष्टसाध्य है, परन्तु अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध हो जाता है।' भगवान के इस कथन पर विचार कीजिए।
व्याख्या - वास्तव में मन तक ही तो सारा आडम्बर है।
यथा-
न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप ।
मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः ।।
(विवेक चूडामणि)
अर्थात् बंध मोक्ष का कारण न देह है, न इन्द्रियाँ और न जीवात्मा है बल्कि सर्व का कारण मन ही है। इसी पर श्री मानसकार भी कहते हैं कि -
योग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥
जनम मरण जहं लगि जग जालू। संपति विपति करम अरु कालू ॥
धरणि धाम धन पुर परिवारू । सरग नरक जहं लगि व्यवहारू ।।
देखिय सुनिय गुनिय मन मांही । मोह मूल परमारथ नाहीं ।।
(रामायण अयोध्या.)
नह्यस्ति विद्या मनसोतिरिक्ता मनोह्यविद्या भववंध हेतुः ।
तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भितेऽस्मिन् सकलं विजृम्भिते ॥
(महोप. उपनिषद)
अर्थात् अविद्या, अज्ञान अथवा सुख-दुःखादि का कारण मन के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। मन के उदय होने पर प्रपंच का उदय है और अस्त होने पर प्रपंच का अस्त है। जीव-ईश्वर का भेद डालने वाला भी तो मन ही है। गाढ़ी नींद, मूर्छा एवं समाधि अवस्था में मन के अभाव में, सर्व का अभाव हो जाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहो कि मन का ही नाम माया है। समष्टि-व्यष्टि भेद से मन अथवा माया दो नाम हो जाते हैं। समष्टि का अर्थ होता है व्यापक और व्यष्टि का अर्थ होता है एकदेशी, यानी देह व्यष्टि जगत् है और समस्त प्रपंच समष्टि जगत् है। जिस प्रकार सागर की एक तरंग और अनेक तरंग, इसी तरह चैतन्याकाश महासागर में एक विकल्प और अनेक विकल्प। विकल्प का पर्याय कल्पना होता है। विकल्प का स्वरूप महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट बतलाया है। महर्षि जी सूत्र लिखते हैं -
शब्दज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः ।
(योगदर्शन)
अर्थात् शब्द का तो ज्ञान हो, परन्तु वस्तु का अभाव हो। यानी केवल शब्द ही सुनने भर में आवे, किन्तु ढूँढ़ने पर जिसका अस्तित्व किसी भी काल में न मिले, उसे कहते हैं विकल्प। मतलब यह कि अस्तित्वहीन वस्तु को ही विकल्प कहते हैं। इसी प्रकार मन, माया अथवा संसार ये श्रोतव्य हैं, प्राप्य नहीं हैं। यानी श्रवण के विषय हैं, प्राप्ति के नहीं। तात्पर्य यह है कि शरीर रूपी व्यष्टि दृष्टि से एक विकल्प का नाम मन है और समस्त प्रपंच रूपी समष्टि जगत् के अन्दर जो अनन्त विकल्प हैं, उन समस्त विकल्पों के समूह का नाम माया है। मतलब यह है कि जो कुछ कहना- सुनना, करना-धरना है वह सब मन के ही अंदर है और मन ही तक है। इसलिए मन की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाये। आइए, भगवान श्री गीताकार के अभ्यास और वैराग्य पर विचार करें, क्योकि योगेश्वर भगवान ने अभ्यास और वैराग्य से ही मन का पकड़ना बतलाया है और महर्षि जी भी सूत्र लिखते हैं कि -
योगश्चित्त वृत्ति निरोधः ॥
(योगदर्शन 1/2)
अर्थात् चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि चित्त का निरोध क्यों अथवा किसलिए करना चाहिए? महर्षि जी कहते हैं कि-
तवाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।।
(योगदर्शन 1/3)
अर्थात् साधक को चित्तद्रष्टा के स्वरूप में स्थान मिल जाता है, यानी चित्त के निरोध में कल्पनाओं का निरोध हो जाता है और कल्पनाओं के निरोध हो जाने पर साधक और चित्त के द्रष्टा, दोनों का भेद मिट जाता है। तात्पर्य यह है कि चित्त की समस्त चेष्टाओं को जो निरंतर देखता है, जानता है तथा अनुभव करता है, यानी चित्त का जो साक्षी है, वही सर्व का अपना आप 'मैं' अपना स्वरूप आत्मा है। इस योग साधक के लिए श्री महर्षि जी ने चित्त का निरोध बतलाया है। यूँ तो आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, सर्व कुछ आत्मा है, परन्तु समस्त कल्पनाओं एवं विचारों के शांत हो जाने पर शुद्ध स्वरूप, उपाधि रहित चेतन 'मैं' नाम से प्रस्फुटित होता है। उस सत्ता पद में साधक स्थित हो जाता है। इसलिए, श्री महर्षि जी के कथनानुसार चित्त निरोध की आवश्यकता है, परन्तु यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, वह यह कि चित्त के निरोध काल तक ही चित्त द्रष्टा की अनुभूति है, शेष काल में तो चित्त ही चित् है। चित्त के निरोध का विकल्प भी चित्त ही तक है। चित्त का अस्तित्व, आत्मा के अज्ञानकाल तक है तथा अज्ञान का अस्तित्व, आत्म जिज्ञासा के अभाव में निहित है। खैर, इस विषय पर फिर विचार करेंगे।
अब चलिए चित्त निरोध के साधन जगत् में।
अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।।
(योगदर्शन)
अर्थात् अभ्यास और वैराग्य से मन अथवा चित्त का निरोध होता है। भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं कि 'अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।' प्रथम अभ्यास एवं वैराग्य का अर्थ करके फिर दोनों की व्याख्या की जायेगी। अभ्यास का मतलब है- 'किसी भी विषय का पुनः-पुनः यानी बार-बार आवर्तन, पुनरावृत्ति करना' और वैराग्य का अर्थ होता है- 'किसी भी देश, काल, वस्तु का त्याग ।
अब प्रश्न यह है कि चित्त निरोध के लिए किस चीज का अभ्यास और किसका त्याग करना चाहिए।
समाधान- अभ्यास न करने का अभ्यास, यही तो अभ्यास है और हो का जो त्याग है, वस्तुतः आत्मा के यह है कि जब तक चित्त का अस्तित्व है, तभी तक प्रपंच काही है। सात्व है और चित्त के अस्तित्व काल तक मन, वचन, कर्म द्वारा चित के हो बिरोध के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है, उसका फल चंचलता के नाश है, चित्त का नाश नहीं। चित्त नाश के दो प्रकार हैं- अरूप नाश और सरूप नाश। सरूप नाश साधन का फल है और अरूप नाश आत्मबोध का फल है। साधन का फल अनित्य होने के कारण सरूप नाश अनित्य है, यानी चित्त का नाश हमेशा के लिए नहीं होता और अपने स्वरूप आत्मा को बोध हो जानेपर चित्त के अस्तित्व का ही नाश हो जाता है। मतलब यह है कि तीन काल में चित्त है ही नहीं, इसको अरूप नाश कहते हैं। इसलिए प्रथम अस्तित्व का त्याग करो। बाद में अभ्यास न करने का अभ्यास करो। यदि करने का अभ्यास करोगे तो वह अभ्यास मन वाणी का विषय होना और जो मन वाणी द्वारा होता है वह स्थाई नहीं होता, बल्कि अस्थाई होता है, इसलिए भगवान कृष्ण के कथनानुसार अभ्यास का अर्थ हुआ अभ्यास न करने का अभ्यास करना, यही अभ्यास है। चित्त अथवा प्रपंच के अस्तित्व का त्याग करना, यही वैराग्य है। क्योकि जब चित्त के अस्तित्व का त्याग ही कर दिया, यनी 'चित्त है' इस विकल्प (कल्पना) का ही जब त्याग हो गया तो जब चित्त ही नहीं रहा, तो निरोध किसका किया जायगा और जब शब्दादिक विषय रूप प्रपंच का ही त्याग हो गया, यानी 'प्रपंच है' इस विकल्प का ही त्याग हो गया तो चित्त जायगा ही कहाँ और किसमें? इस प्रकार का त्याग ही वास्तविक व्याग है और यही सर्व व्याग है। इसी त्याग को श्री मानसकार के शब्दों में परम वैराग्य कहते हैं।
वैराग्य दो प्रकार का होता है- एक अपर वैराग्य, दूसरा पर वैराग्या जो वैराग्य आत्मबोध के प्रथम होता है, उसे अपर वैराग्य कहते हैं और जो बोध के पश्चात् होता है, उसे पर-वैराग्य कहते हैं। यथा -
जानिय तबहिं जीव जग जागा । जब सब विषय विलास विरागा ।।
यह अपर वैराग्य है। और -
कहिय तात सो परम विराणी । तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी ।।
यह पर वैराग्य है।
बोध के प्रथम शब्दादिक विषयों के विलास, यानी भोग का व्याग होता है और बोध हो जाने पर विषयों के अस्तित्व का ही व्याग हो जाता है। आत्मानुभव के प्रथम सत् शास्त्र और महान् पुरुषों के सत्संग द्वारा आत्मा नित्य है, जगत् अनित्य है - ऐसे विवेक एवं विचार से प्रपंच में दोष दृष्टि पैदा हो जाती है, प्रपंच की नश्वरता प्रतीत होने लग जाती है। उस समय संसार से चित्त खिन्न हो जाने पर, जीव विषय के विलास (भोग) का त्याग कर देता है, विषय का नहीं। इसे अपर वैराग्य कहते हैं। अब यह भी दो प्रकार का होता है- एक सोपाधिक, दूसरा निरुपाधिक। सोपाधिक वैराग्य का लक्षण यह है कि संसार में स्त्री-पुत्र, धन-कलत्र अथवा चिरकालीन शारीरिक रोग इत्यादि से चित्त में विक्षेप पैदा हो जाने से प्रपंच के विलास का जो त्याग होता है, उसे अपर वैराग्य कहते हैं। परन्तु, अपर वैराग्यवान व्यक्ति के लिए श्रुति-स्मृति, सन्त-महात्माओं ने जगत् में भ्रमण करने के लिए निषेध किया है, क्योंकि जिन विषयों के भोग से वैराग्य हुआ है, वे सब विषय अन्तःकरण में अभी तक अधिकार जमाये बैठे हैं और जगत् प्रपंच में विचरने से संग दोष के कारण फिर भी विषयों में आसक्त हो जाना कोई असंभव नहीं है। इसलिए अपर वैरागी को चाहिए कि एकान्त सेवन करते हुए खुष्ठ न्याय के समान अपर वैराग्य को पकावे। खुष्ठ न्याय का मतलब यह होता है कि (खुष्ठ कहते हैं खूँटे को) जिस तरह खूँटे को जमीन में गाड़ते समय बार-बार ठोकर मारना और फिर हिलाकर उसकी मजबूती देखी जाती है, इसलिए कि जो भी पशु बांधा जाय वह कहीं उखाड़कर भाग न जाय, इसी प्रकार एकान्त सेवन, सत् शास्त्र (वेदान्त) का विचार एवं सत्पुरुषों का सत्संग करते रहना चाहिए और निरन्तर कोशिश करते रहना चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र अपने स्वरूप आत्मा का बोध हो जाय। अब निरुपाधिक वैराग्य का लक्षण सुनो। वैराग्य में किसी तरह की उपाधि अथवा चित्त में विक्षेप नहीं है, परन्तु अनन्त जन्मों का पुण्य उदय होने पर वीतराग अर्थात् विरक्त पुरुषों का समागम होता है और संतों की कृपा से बुद्धि में नित्यानित्य का विवेक होता है, तब ऐसे विवेक एवं विचार द्वारा प्रपंच के भोग से जो वैराग्य पैदा होता है उसे निरुपाधिक वैराग्य कहते हैं। परन्तु, ऐसा निरुपाधिक वैराग्य बिरले ही मनुष्य को हुआ करता है, सबको नहीं। इस प्रकार सोपाधिक एवं निरुपाधिक वैराग्य आत्मानुभूति के प्रथम हुआ करता है।
अब पर या परम वैराग्य का लक्षण सुनो। पर वैराग्य में, विषयों के अस्तित्व का त्याग हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जिनको विषय मानता था वस्तुतः वे विषय, विषय नहीं हैं, 'मैं' आत्मा हूँ। देह, इन्द्रिय, मन, प्राण तथा शब्दादिक विषय अथवा सारा प्रपंच तीन काल में है ही नहीं, 'मैं' ही 'मैं' हूँ। जब सर्व में ही हूँ, इस प्रकार का बोध होता है तो उस समय में आत्मा के अतिरिक्त, सर्व के अस्तित्व का ही त्याग हो जाता है और जब चित्त के अस्तित्व का ही त्याग हो गया, यानी जिसको मन या चित्त कहते हैं, वह मन के रूप में 'मैं' ही हूँ, जिस तरह जल में तरंग, ऐसी अनुभूति हो जाने पर भला निरोध किसका किया जाय और कौन निरोध करेगा। यथा-
पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तये दोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत् ।
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ॥
(अ.रा. रामगीता 48)
अर्थात् भगवान राम, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आत्म-कल्याण के साधक को चाहिए कि निर्विकल्प समाधि सिद्धि के प्रथम साधक ऐसा चिंतन करे कि ब्रह्मा से आदि तृण पर्यन्त सब कुछ ब्रह्म है। यानी, सर्व 'मैं' हूँ, क्योकि जगत् प्रपंच वाच्य है। प्रणव 'ऊँ' आत्मा वाचक है, जैसे आभूषण वाच्य है, स्वर्ण वाचक है। वस्त्र वाच्य, धागा वाचक है। घट वाच्य है, मिट्टी वाचक है। इसी तरह स्थूल, सूक्ष्म, कारण जगत् प्रपंच वाच्य है और 'मैं' आत्मा इसका वाचक हूँ। अज्ञान दृष्टि में प्रपंच अथवा देहादिक प्रपंच भास रहा है, आटम दृष्टि में नहीं। भगवान श्रीराम ने इस प्रकार सरल तथा विलक्षण साधन चित्त को निर्विकल्प करने के लिए बतलाया है। यथा -
यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषुक्वचित् ।
पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥
(भाग. 4/7 / 53 )
जिस प्रकार हाथ-पैर, आँख-कान, मुख-शिर इत्यादि सब अंगों के सहित होने पर ही मनुष्य संज्ञा होती है, यानी मनुष्य कहलाता है, जैसे और सब अंग तो हैं, परन्तु एक अंग भी जरा-सा भंग हो जाय तो वह खंडित मनुष्य कहा जाता है, अंगहीन कहलाता है। इसी प्रकार एक तृण को भी भगवान से जहाँ भिन्न माना कि भगवान खण्डित हो गया। वेद, शास्त्र, संत, महात्मा गण एवं स्वानुभूति से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि परमात्मा अखण्ड है और उपासना जगत् में भी यही नियम है कि कोई भी मूर्ति जरा- सी खण्डित हो जाने पर पूजन के योग्य नहीं रहती। यानी शास्त्र में खण्डित मूर्ति के पूजने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि परमात्मा अखण्ड है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह व्यक्ति सब अंगों के सहित मनुष्य कहलाता है, इसी तरह समस्त चराचर के सहित भगवान की अखण्डता सिद्ध होती है। इसलिए 'मैं' आत्मा सर्व हूँ यह चिंतन अथवा निश्चय काल्पनिक या भावनात्मक नहीं बल्कि वास्तविक है।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।
(गीता 6/30)
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।।
(गीता 6/31)
अर्थात् जो पुरुष सारे चराचर में मुझ आत्म स्वरूप यानी 'मैं' को अथवा सारे चराचर को 'मैं' आत्मा देखता है, उससे न 'मैं' भिन्न हूँ और न वह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार जो सर्व में तथा सर्वत्र एक भाव से, यानी 'मैं' सब में हूँ और 'मैं' सब कुछ हूँ, इस भाव से भजता अर्थात् जानता है वह सब व्यवहार में वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। यानी उसकी दृष्टि में व्यवहार, परमार्थ दोनों है ही नहीं, केवल 'मैं' ही 'मैं' हूँ।
शनैः शनै रुपरमे द्बुद्धया धृतिगृहीतया ।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥
(गीता 6/25)
अर्थात् धीरे-धीरे मन को विषयों से उपराम करे। मतलब यह कि जिस समय जिस विषय में मन जाय, उस समय उस विषय को विषय न मानकर अपना स्वरूप भगवान आत्मा जानना चाहिए। यानी विषयों के अस्तित्व का त्याग ही कर देना चाहिए। विषयों से मन का यही उपराम है और मन को परमात्मा में इसी प्रकार स्थित करना है और कुछ भी चिंतन न करो जिस प्रकार सर्प के चिंतन से सर्प नहीं मरता, बल्कि रज्जू के ही चिंतन से सर्प मरता है, इसी तरह चित्त अथवा सर्प विषय के चिंतन से विषयों का नाश नहीं होता बल्कि 'मैं' भगवान आत्मा के ही चिंतन से चित्त अथवा विषय प्रपंच का नाश होता है। यूँ कहो कि चित्त और विषय दो चीज नहीं है, बल्कि 2 चित्त का ही नाम विषय है। चित्त ही विषय और विषय ही चित्त है। जिस प्रकार मकड़ी अपने ही अंदर से जाला बनाकर अपने आप उसमें फँस जाती है. अपने आप से, अपने इरल बनकर अपने आप ही मकड़ी के समान फँस जाता है। इसलिए जहय जाहाँ पर मन जाय, वहाँ-वहाँ पर अपने आपको ही देखो। मन है उड़ने वाला, कल्पना है उड़न खटोला और शब्दादिक पाँचों विषय एरोड्रम यानी हवाई अड्डे हैं। इसलिए उड़न-बाज मन के सहित कल्पना रूपी राकेट तथा विषय रूपी अड्डों को परम वैराग्य रूपी एटम बम से भुन दो, खाक कर दो, इनकी हस्ती मिटा दो। मन रूपी गाड़ी के संकल्प-विकल्प दोनों चक्के निकाल दो। चारों तरफ की सारी लाइनें काट दो। तभी तो आजादी है, नहीं तो जीवन की बरबादी है। ऐसी बमबारी से कुछ भी शेष नहीं रहता। हाँ, जो शेष है, वही शेष रहता है।
देहाभिमाने गलिते स्वरूपे परमात्मनि ।
यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः ।।
(पंचदशी)
अर्थात् अपने स्वरूप परमात्मा में देहाभिमान गलित हो जाने पर जहाँ- जहाँ पर मन जाय, वहाँ-वहाँ पर भगवान आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है बीक ही नहीं क्योंकि -
एतावानात्मसम्मोहो यद् विकल्पस्तु केवले ।
आत्मभृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि ।।
(भागवत 11/28/36) अस
अर्थात् यह कैसा आत्म सम्मोह है कि कैवल्य, चैतन्य घनभूत 'मैं' में चित्त का विकल्प हुआ, जैसे रज्जु में सर्प का विकल्प होना। यह रज्जु अ विषयक मोह है। इसी तरह अपने स्वरूप आत्मा से किंचित् मात्र एक तृण ओट को भी जहाँ भिन्न माना, वहीं पर आत्मा विषयक मोह आ गया। मतलब यह है कि विकल्प का कोई न कोई आधार जरूर होता है। रज्जु यदि न हो तो सर्प का विकल्प किसमें होगा? इसी प्रकार यदि 'मैं' न होऊँ तो पंच महाभूत, देह, इन्द्रिय, मन, प्राण अथवा सारे प्रपंच इन सबों की कल्पना किस पर और किसमें होगी अथवा इनकी कल्पना करने वाला कौन होगा? इसलिए सर्प का अवलम्ब यानी आधार 'मैं' आत्मा ही हूँ, दूसरा कोई नहीं।
मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः ।
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमत्रजसा ।।
(भावा. 11/13 / 24 )
अर्थात् भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मन, वचन, दृष्टि तथा इन्द्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह सब 'मैं' आटमा ही हूँ, मुझ से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसे सरलतापूर्वक तुम समझ लो।
तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ।।
(ब्रह्म सूत्र 1/10)
अर्थात् सूत्रकार भगवान श्री व्यास जी कहते हैं कि सर्व का कारण जो ब्रह्म है उसके जानने वाले का ही मोक्ष होता है।
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य ।
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत् ।।
(भाग. 11/28/19)
अर्थात् जैसे पहले भी सोना बाद में भी सोना, बीच में नाम रूपात्मक जो आभूषण है वह भी सोना ही है। इसी प्रकार पहले भी 'मैं' बाद में भी 'मैं' और बीच में ब्रह्मा से आदि तृण पर्यन्त सारा चराचर, जो आभूषण के समान भास रहा है, यह भी सर्व 'मैं' आत्मा ही हूँ। तात्पर्य यह है कि जैसे वस्तु अविद्यमान यानी न होते हुए और भासती है (जैसे- सर्प अविद्यमान यानी न होते हुए अंधकार के कारण भासता है, वास्तव में वह सर्प तीन काल में नहीं है, असलियत में रज्जु ही है जो कि सर्प के आकार में भासती है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण रज्जु में सर्प के समान प्रपंच, जो भास रहा है, सो प्रपंच अथवा चित्त किसी काल, किसी अवस्था में नहीं है, बल्कि 'मैं' भगवान आत्मा ही हूँ।
यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातꣲ᳜ स्याद्वाचारम्भणं ।
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥
(छा 6/1 / 4 )
अर्थात् जिस प्रकार एक मृत्तिका पिंड को जान लेने पर मिट्टी से बने हुए समस्त घट आदि पदार्थों का ज्ञान हो जाता है (यानी सब मिट्टी ही है)। उसी प्रकार घट आदि विकार तो केवल कथन के लिए है, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है।
यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातꣲ᳜ स्याद्वाचारम्भणं ।
विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥
(छां.उ..6 / 1 / 5)
अर्थात् जिस प्रकार लोहे के एक टुकड़े का ज्ञान होने पर लोहे के बने हुए सभी पदार्थों का ज्ञान हो जाता है (यानी ये सब शस्त्रादिक तो लोहा ही है) उसी प्रकार नाम रूप तो केवल वाणी के विकार मात्र हैं, सत्य तो लोहा ही है।
यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन
सर्वकार्णायसं विज्ञातꣲ᳜ स्याद्वाचारम्भणं ।
विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव
सत्यमेवꣲ᳜ सोम्य स आदेशोभवतीति ॥
(छां.उ..6 / 1 / 6)
अर्थात् जिस प्रकार एक नहन्ना के ज्ञान से लोहे से बने हुए समस्त खड्ग आदि शस्त्रों का ज्ञान हो जाता है, क्योकि शस्त्र आदि विकार तो केवल नाममात्र वाणी पर ही अवलम्बित है, सत्य तो लोहा ही है।
स एवेदꣲ᳜ सर्वम् ।।
(छां.उ..7 / 25 / 1)
अर्थात् सर्व वही है।
अहमेवेदꣲ᳜ सर्वम् ।।
(छां.उ. 7/25 / 1 )
अर्थात् सर्व 'मैं' ही हूँ।
आत्मैवेदꣲ᳜ सर्वम् ।।
(छां.उ. 7/25/1)
अर्थात् सर्व आत्मा ही है।
इन श्रुतियों के कथन से भी यही सिद्ध होता है कि नाम रूपात्मक जो संसार भास रहा है, यह केवल नाम मात्र वाणी पर ही अवलम्बित है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सत्य तो केवल 'मैं' आत्मा ही हूँ। आश्चर्य तो यह कि सारा तमाशा मन तक ही है और यहाँ तक कि मन खुद ही तमाशा है।
मनो दृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरम् ।
मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ।।
(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र. 31)
अर्थात् जो कुछ भी चराचर द्वैत है अथवा दृश्य है, यह सब मन ही है। मन जब अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है तब द्वैत प्रपंच का लेश भी नहीं रहता।
आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा ।
अमनस्तां तदा याति ग्राह्यभावे तद्यहम् ।।
(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र. 32)
अर्थात् जब सत्य सनातन आत्मा की अनुभूति हो जाती है, उस समय यह मन संकल्प नहीं करता अर्थात् संकल्प और विकल्प से रहित हो जाता है।
निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः ।
प्रचारः सतुविज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः ।।
(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र. 34)
अर्थात् मन के निग्रह हो जाने पर निर्विकल्प भाव आ जाता है। वह अवस्था जानने योग्य है। यानी कल्पना रहित अवस्था में शेष क्या रह जाता है, इसे जानना चाहिए। परन्तु, सुषुप्ति (गाढ़ी) निद्रा में ऐसा नहीं है क्योंकि, उस अवस्था में मन अज्ञान में लय होता है। जागने पर कहता है कि आज मैं ऐसा सोया, कुछ पता ही नहीं रहा, यही अज्ञान का स्वरूप है। यद्यपि सोया नहीं, परन्तु कहता है कि मैं सोया। इस अज्ञान में मन लय होता है।
लीयते हि सुषुसे तदभिन्गृहीतं ।
तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥
(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र. 35)
अर्थात् सुषुप्ति अवस्था में मन अविद्या में लीन होता है। किन्तु निरोध हो जाने पर वह मन उसमें लीन नहीं होता। उस समय तो सब प्रकार से या सर्व और से निर्भय बहा ही रहता है। इसलिए सुषुप्ति और समाधि में भेद है, क्यो सर्व अगर के निरोध का ही नाम समाधि है और मन के अज्ञान में लय होने का नाम सुबत्ति है। सुषुप्ति अवस्था तमोगुण का कार्य है, और समाधि शुद्ध सतोगुण सुषकार्य है, इसलिए भी सुषुप्ति और समाधि में अंतर है। दूसरी बात है कि योगियों का अक्षय सुख तो समाधि तक ही सीमित है।
मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्व योगिनाम् ।
दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेवच ॥
(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र.)
योगियों के योग साधन की पराकाष्ठा अथवा समस्त साधनों की परिसमाप्ति चित्त के निर्विकल्प समाधि की सिद्धि में ही निहित है। समाधि में परम् तत्व का बोध, अष्ट पाश से मुक्ति, पंच क्लेशों से निवृत्ति, सर्व दुःखों का क्षय तथा अक्षय शान्ति पद की प्राप्ति है। परन्तु, आत्मवेत्ता पुरुष के आत्म-देश में सविकल्प, निर्विकल्प दोनों का विकल्प तीन काल में है ही नहीं। स्वदेश में तो निर्भयता है।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति ॥
(तैत्तरीय उप 2/4 / 1 )
श्रुति कहती है कि जहाँ से मन सहित वाणी लौट आती है यानी मन जिसका मनन नहीं कर सकता, वाणी जिसका कथन नहीं कर सकती -
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ॥
(केन.3.1/5)
यद्वाचानभ्युदितः ॥
(केन.3.1/4)
ऐसा जो सत्य सनातन ब्रह्म है, उसके आनन्द को पाकर विद्वान ब्रह्मवेत्ता पुरुष सर्व से निर्भय हो जाता है।
प्रश्न-क्यों निर्भय हो जाता है, यानी किसी के भय क्यों नहीं करता?
समाधान-भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः ।
भीषाऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमेति ॥
(वैत्तिरी.उ. ब. ब. अनु. 9, मं. 1)
अर्थात् जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य उदय होता है, इन्द्र वर्षा करता है और अग्नि काष्ठ को वहन करती है तथा मृत्यु उत्पन्नशील पदार्थ को खाने के लिए दौड़ता है, सारांश यह कि सारा विश्व भयभीत होता है, उस सनातनतत्व विश्वात्मा, सर्व के सर्व 'मैं' संज्ञा से अभिव्यक्त ब्रह्म को प्राप्त करके विद्वान किसी से भी भय नहीं करता, यानी निर्भय को पाकर निर्भय हो जाता है। जिस समय मन संकल्प-विकल्प से रहित हो जाता है, उस समय केवल निर्भय सत्ता ही रह जाती है। और वैसे तो -
चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च ।
अभूतो हियतश्चार्थो नार्थाभासस्ततःपृथक् ।।
(गौ.पा.का. अला.प्र. 26)
अर्थात् चित्त न किसी पदार्थ का अथवा उस पदार्थ के अर्थ को ही कभी स्पर्श करता है, क्योंकि भासने वाले जो पदार्थ हैं, उनकी चित्त से पृथक सत्ता नहीं है। यानी चित्त से भिन्न नहीं है। सारांश यह है कि सारा चराचर ही चित्त है। चूँकि सुषुप्ति, समाधि एवं मूर्च्छाकाल में चित्त के अभाव हो जाने पर न तो पदार्थ का भान होता है और न उस पदार्थ के अर्थ का ही भान होता है, अतः, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चित्त ही सारा प्रपंच है और प्रपंच ही चित्त है। चित्त के उदय में प्रपंच का उदय है और अस्त में प्रपंच का अस्त है। इसलिए चित्त से भिन्न प्रपंच तीन काल में है ही नहीं। तब चित्त किसका स्पर्श करेगा? यानी किसमें और कब तथा क्यों जायेगा? फिर दूसरी बात यह है कि चित्त भी नहीं है, यानी न तो चित्त है और न चित्त का दृश्य ही है। सारांश यह है कि आत्मा का विकल्प चित्त है और चित्त का विकल्प, चित्त का दृश्य अर्थात् चराचर प्रपंच है।
तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते ।
तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वैपश्यन्ति ते पदम् ।।
(गौ.पा.का.अ.शा.प्र. 28)
इसलिए न चित्त उत्पन्न होता है, न चित्त का दृश्या चित्त और चित्त के दृश्य को जो उत्पन्न होना देखते हैं, वे मानो निश्चय ही आकाश में पक्षी के चरण चिह्न देखते हैं। यानी निराधार सूक्ष्म आकाश में पक्षी के चरण चिह्न नहीं दिखाई पड़ते। परन्तु, अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार आकाश में पक्षी के चरण चिह्न देखने की कल्पना करें कि हमको आकाश में पक्षी के चरण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार किसी भी अवस्था में न तो चित्त है और न चित्त का दृश्य ही है। फिर कौन है? अरे, वही है जो चित्त का चित्त है, दृश्य का दृश्य और सर्व का सर्व है।
प्राण प्राण के जीव के, जिय सुख के सुख राम ।।
(रामायण अयोध्या.)
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्भाचोहवाच स उ प्राणस्य प्राणः ॥
(के.उ.1/2)
अर्थात जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, यानी जो सर्व का सर्व है। जैसे- जल के बिना तरंग नहीं, तो जल हुआ तरंग का सर्वी तात्पर्य यह है कि वही उसका सर्वस्व होता है, जो उसे सिद्ध करता है। 'में' (आत्मा) से भिन्न कर लेने पर किसी भी देश, काल, वस्तु का अस्तित्व रहता ही नहीं। 'मैं' से भिन्न न चित्त है, न चित्त का दृश्य ही है, परन्तु चित्त तथा दृश्य (प्रपंच) की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। जिस तरह तरंग देश में तरंग है, जल देश में तरंग तीन काल में नहीं, इसी तरह चित्त अथवा मन देश में मन है। आत्म देश में न मन है और न मन से उत्पन्न होने वाले वैकल्पिक विकार रूप दृश्यादिक पदार्थ है।
अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते ।
वस्त्वभावं स बुद्ध्चैव निःसंगं निविवर्तते ॥
(गौ.पा.का. अला.शा.प्र. 79)
अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले मन को जिस काल में यह बोध हो जाता है कि आत्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, उसी क्षण मन अपने आप स्वरूप आत्मा में लौट आता है। बोधवान मन को फिर रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारांश यह है कि अपने आप में, अपने आप करके, अपने आपको 'मैं' से भिन्न कुछ भी मानना ही मन है और जब मन बन गया, तब सभी कुछ भासने लगा। दुनिया के लोग देह के नाश को [आत्मघात कहते हैं। अरे अज्ञानियों! यह पंचभौतिक शरीर को किसी प्रकार से भी नाश कर देने का नाम आत्मघात अथवा आत्महत्या नहीं है। बल्कि, स्वरूप आत्मा को आत्मा न जानकर, आत्मा को कुछ भी मान लेना बस यही आत्महत्या है और ऐसा जो करता है वही आत्मघाती है। कैसा अचम्भा है। खेल, खिलौना, खिलाड़ी तथा देखने वाला सब कुछ खुद ही है और नहीं तो सच्चाई अथवा ईमानदारी तो यह है कि - -
स्वतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते ।
सवसत्सवसद्वापि न किंचिद्वस्तु जायते ।।
(गौ.पा.का.अ.शा.प्र. 22)
अर्थात् न सत् की उत्पत्ति होती है, न असत् ही उत्पन्न होता है और न सद्, असत् दोनों की ही उत्पत्ति होती है। यदि सत् पदार्थ की उत्पति मानोगे तो उत्पन्न हुआ पदार्थ नाशवान होता है। फिर इसे सत् कैसे कहेंगे? क्योंकि सत् वस्तु त्रिकालाबाध्य होती है और यदि असत् की उत्पत्ति मानोगे तो असत् बंध्या पुत्रवत् होता है। यानी जो है ही नहीं, वह पैदा क्या होगा। तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार से भी किसी भी देश, काल, वस्तु का उत्पन्न होना किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। 1. प्रत्यक्ष प्रमाण, 2. अनुमान प्रमाण, 3. श्रुतिशास्त्र प्रमाण एवं 4. स्वानुभूति प्रमाण। इन चारों प्रमाणों से जो सिद्ध हो, वहीं न्याय है और वही सार्वभौम सिद्धान्त है। दूसरी चीज यह है कि सत्, असत् और सत्-असत् दोनों, यदि इनका जन्म माना जाय तो माया देश में है। माया का अधिष्ठान आत्म देश में नहीं है। क्योंकि, माया का अर्थ होता है अज्ञान, यानी सत् देश में सत् का जन्म नहीं, सत् के अज्ञान देश में सत् का जन्म है। असत् देश में असत् का जन्म नहीं, असत् के अज्ञान देश में असत् का जन्म है। इसी तरह सत्-असत् देश में सत्-असत् का जन्म नहीं, बल्कि सत्-असत् के अज्ञान देश में सत्-असत् का जन्म माना जा सकता है।
सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः ।
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥
असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते ।
बंध्या पुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥
(गौ.पा.का. अद्वैत.प्र. 27, 28)
जैसे रज्जु का सर्प रज्जु देश में न सत् है, न असत् है और न सत्-असत् दोनों है। रज्जु के अज्ञान देश में सर्प सत् भी है, असत् भी है और सत्-असत् दोनों भी है।
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ॥
(बृ.3.2/5/19)
इन्द्र माया करके अनेक रूप धारण करता है। माया को श्रुति अजा नाम से प्रतिपादित करती है।
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।।
(श्वेता.उप. 4/5)
अर्थात् जो जन्म रहित हो उसे अजा कहते हैं।
अजो होको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोऽन्यः ॥
(श्वे.3.4/5)
अर्थात् अपने अनुरूप ही लोहित (लाल), शुक्ल (सफेद), कृष्ण (काला) वर्णवाली, सत्-रज-तम तीन गुण वाली प्रकृति कभी भी जन्म न लेने वाली अजा प्रकृति माया को एक अज (अजन्मा) जीव सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा अज (अजन्मा) ईश्वर त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया को त्याग देता है। इस श्रुति प्रमाण से जीव, ईश्वर तथा प्रकृति तीनों अजन्मा है। सारांश यह है कि किसी काल में किसी का भी जन्म नहीं सिद्ध होता। वेदान्त शास्त्र में इसको ही 'अजातवाद' कहते हैं।
ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा होका भोक्तृभोगार्थयुक्ता ।
अनन्तश्चाटमा विश्वरूपोह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥
(श्वे.उ.1 / 9)
अर्थात् ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर समर्थ है, जीव असमर्थ है। ईश्वर अकर्ता एवं अभोक्ता है, जीव कर्त्ता-भोक्ता है। ईश्वर एक है, जीव अनेक है। यह सब होने के बावजूद ये तीनों अजन्मा हैं और अजन्मा होने से तीनों सत् हैं। सन् होने से तीनों चित् हैं और चित् होने से ये तीनों आनन्दस्वरूप हैं। इस प्रकार इन तीनों को जो सत्, चित्, आनन्द रूप अद्वितीय सनातन ब्रह्म आत्मा अपना आप, साक्षात् अपरोक्ष 'मैं' जानता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। यानी तीनों को सिद्ध करने वाला कौन? सर्व का सर्व 'मैं', ऐसा जानकर कृतार्थ हो जाता है। सारांश यह है कि जिस करके जो सिद्ध होता है वह सिद्ध होने वाला पदार्थ सिद्ध करने वाले से भिन्न नहीं होता।
अब यहाँ पर विचारणीय विषय है कि जीव, ईश्वर, प्रकृति को सिद्ध कौन करता है? जीव का मैं, ईश्वर का मैं या प्रकृति का मैं इन तीनों में जो 'मैं' है वह कौन है? अरे भाई, वह वही है जो जीव को अल्पज्ञ मानता है, ईश्वर को सर्वज्ञ मानता है और प्रकृति को नाना नाम रूप जगत् मानता है। परन्तु जो सर्व को मानता है, उसे कौन मानता है? जो सर्व vec aD देखता है, उसे कौन देखता है? अतः, सर्व के मानने वाले का मानने वाला दूसरा नहीं, सर्व के जानने वाले का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं, सर्व के देखने वाले का दृष्टा उससे भिन्न कोई नहीं। इसलिए जीव, ईश्वर और प्रकृति इन तीनों में जो सत् का सत् है, चित् का चित् है तथा आनन्द का जो आनन्द है, वह कौन है? वह 'मैं' है।
अब प्रश्न होता है कि 'मैं' क्या है?
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ।।
(गीता 15/19)
अर्थात् जो ज्ञानवान मुझको ही यानी अपने आप 'मैं' को ही पुरुषोत्तम 'मैं' जानता है, वह सर्वरूप 'मैं' का वेत्ता, सर्वभाव से मुझ परमात्मा को ही भजता है। इसलिए 'चंचलं हि मनः कृष्ण' अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने इस प्रकार से दिया कि 'अभ्यासेनतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।' यानी मन के अस्तित्व का जो त्याग है, यही वैराग्य है और अभाव रूप मन के लिए कुछ भी न करना ही अभ्यास है। हाँ, अपने को जीव मानते हो तो मन के लिए कुछ करो और मरो और यदि मैं को 'मैं' ही (आत्मा) जानते हो तो न करो न मरो। मस्त रहो।
3.तस्मात्सर्वेषु कालेषु
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मटयर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ।।
(गीता 8/7)
भगवान् अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तू मुझे सर्वकाल में भज। सर्वकाल में भजन करना क्या है? आज सुबह जब सोकर उठे तो उस समय घड़ी में क्या बजा था? करीबन चार बजे होंगे। जब चार बजा था उस समय मैं था कि नहीं? था। क्या प्रमाण है? अरे, उस वक्त में न होता तो चार बजा था उसे कौन देखता। फिर चार से पाँच, पाँच से छः, छः से सात बजा। काल का इतना वेग है कि क्षण-प्रतिक्षण भविष्य वर्तमान हो रहा है और वर्तमान भूत हो रहा है। अभी हूँ कि नहीं, क्या प्रमाण है? देख रहा हूँ और शाम को पाँच बजे रहूँगा कि नहीं, हाँ तब भी रहूँगा। स्वप्न काल में रहता हूँ कि नहीं? रहता हूँ। यदि मैं न रहूँगा तो स्वप्न का साक्षी कौन होगा कि स्वप्न देखा, उस समय कोई और रहता है क्या? नहीं, मैं ही रहता हूँ। मैं स्वप्न में भी रहता हूँ और जाग्रत में भी रहता हूँ। जो मैं, जैसा मैं और जिस प्रकार मैं जायत अवस्था में रहता हूँ वहीं मैं, वैसा ही मैं, उसी प्रकार मैं स्वप्न अवस्था में और जो मैं, जैसा में स्वप्न में, वैसा ही में, वही में, सुषुप्ति अवस्था में। जैसा मैं सत् रूप से, वैसा ही चित् रूप से और उसी प्रकार आनन्द रूप से मैं सदैव तीनों काल, तीनों अवस्था में हूँ, तो फिर मैं हूँ इसमें तो कोई शंका नहीं है। भाई देखो, जब पहले भगवान को जान लोगे तब तो उनका स्मरण करोगे। कोई ऐसा टाइम है, जिसमें मैं न रहूँ। कोई ऐसी वस्तु है, जिसको मैं न देखें। मैं सर्वकाल में हूँ, सर्वअवस्था के प्रपंच को जानता हूँ, देखता हूँ और परम प्रिय हूँ। इसलिए सर्वकाल में रहने वाला हूँ 'मैं'। यह देह नहीं, पंच भौतिक शरीर, लिंग शरीर आदि नहीं। यह तो नाशवान है। तब भगवान का स्मरण सर्वकाल में रहने वाली चीज जो आत्मा है, इससे इसी का सर्वकाल में स्मरण हो सकता है।
इस श्लोक की जो व्याख्या की जा रही है, इसका यही अर्थ होगा और अन्य जो अर्थ होगा वह सब अनर्थ होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। आत्मा में आत्मा का ही सर्वकाल में स्मरण हो सकता है, अनात्मा का नहीं। इसलिए यदि विद्वान हो तो वेदों-शास्त्रों का प्रमाण लो और यदि अपढ़ हो, पढ़े-लिखे नहीं हो तो युक्तियों का प्रमाण लो और यदि श्रद्धालु हो तो महान पुरुषों के वाक्यों को मानो- जो 'मैं' से भिन्न है, वह भगवान नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 'मैं' अपने स्वस्वरूप आत्मा से जो भिन्न है, वह भगवान नहीं है। यदि भिन्न मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही है। जो 'मैं' से भिन्न है वह भगवान नहीं है, यह निश्चय करके बताया गया है। जिसे तीन प्रमाण प्रमाणित करे वही सत्य माना जाता है। साढ़े तीन हाथ का भगवान नहीं, हड्डी, चमड़ा, मांस का टुकड़ा नहीं, इससे परे आत्मा। 'मैं' वही चैतन्य ब्रह्म है।
स्वामी जी, स्मरण का क्या स्वरूप है? सर्वकाल में स्मरण कैसे करें?
भगवान कहते हैं कि सर्वकाल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। भैया! संसार के जितने भी चिंतन हैं, वे चिंतन चिंतनीय हैं। संसारी पदार्थों का चिंतन होता है, परन्तु भगवान अचिंत्य हैं। अचिंत्य का चिंतन मन से नहीं होता, बुद्धि से नहीं होता। अचिंत्य का चिंतन, मन वाणी का विषय नहीं है। देखो, यह मन है, इसको कौन जानता है? 'मैं' जानता हूँ। 'मैं' ही मन का अनुभव करता हूँ, तो 'मैं' का मन कैसे अनुभव करेगा? मन से परे मैं का स्मरण होता है, जिस प्रकार प्रकाश करके प्रकाश देखा जाता है। उसी तरह मैं करके मैं का अनुभव होता है।
एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते ॥
भागवत् 10/14/24
जिस तरह प्रकाश से प्रकाश देखा जाता है, उसी प्रकार मैं, से मैं का चिंतन होता है। भगवान मन, वाणी का विषय नहीं है। भगवान मन से परे, वाणी से परे, बुद्धि से परे है। तो उस भगवान का चिंतन मन से कैसे हो? स्वामी जी, चिंतन का क्या स्वरूप है? भैया देखो, जो चित्त द्वारा चिंतन और स्मरण होता है वह चिंतन, स्मरण मैं (आत्मा) का नहीं है। इस बोध में तो कोई कसर नहीं है कि मैं सच्चिदानन्द आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ। अच्छा, अब स्मरण किसका करोगे? (स्वामी जी ध्यानमग्न हो जाते हैं), बस, यही स्मरण है। ठोस, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। सर्वकाल में अस्तित्ववान मैं आटमा हूँ। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में, जायत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में, मैं अस्तित्ववान आत्मा हूँ। इस निश्चय में तो कोई कमी नहीं है। अब ऐसी क्या चीज है, जिसके चिंतन और स्मरण का विकल्प करते हो। जब इस डण्डे को यह निश्चय हो गया कि मैं डण्डा नहीं हूँ, मैं लकड़ी हूँ, तो मैं लकड़ी हूँ, मैं लकड़ी हूँ इसकी माला फेरने की क्या जरूरत है। जब इसे पूर्ण बोध हो गया कि में आत्मा हूँ, तो यह निश्चय सर्वकाल में, सर्वकाल के लिए हो गया। अब क्या यह प्रयास सिद्ध है या अपने आप है। बस, सहज भाव में आ गया। भगवान का यह कथन क्या साधारण कथन है। यह तो स्वभाव का कथन है। सहजावस्था है, न जीव भाव है, न ब्रह्म भाव है, कुछ नहीं है। तो ऐसा जो स्मरण है वह सर्वकाल में होगा कि एक काल में? सर्वकाल में। जब तुम ब्राह्मण हो, तो क्या तुम ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ करके जप करते हो या जब आँख बन्द करके बैठते हो तब ब्राह्मण रहते हो, उसी तरह इस तत्त्व का यही बोध हो जाने से कि 'मैं' आत्मा सत् हूँ, चित् हूँ और आनन्द स्वरूप हूँ। इसका स्मरण है।
जाग्रन निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥
किसी भी विषय का अनुभव तुम जाग्रत में करते हो या सुषुप्ति में या जाबत और सुषुप्ति से परे अवस्था में। चित्त की चंचलता का नाम है जायत और चित्त के लय का नाम है सुषुप्ति। मन की चंचल अवस्था में और विक्षिप्त अवस्था में सुन ही नहीं सकते और मन के लय अवस्था में भी सुन नहीं सकते, यहाँ तक कि कोई भी काम नहीं हो सकता। अब इन तीनों अवस्थाओं में भगवत् स्मरण नहीं होता और सहजावस्था इससे परे की अवस्था है। अहर्निश स्वरूपस्थ होकर ही युद्ध करोगे, स्वरूप से विलग होकर नहीं। स्वरुपस्थिति का नाम ही भगवत् स्मरण है। यही एक रस स्थिति है भैया, जो बिना बनाए अपने आप बनी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। खैर, मान लो कि तुम विद्वान हो, विचारशील हो, सत्संगी हो, विषय को समझते हो, परन्तु जो बिल्कुल विचार करने वाले नहीं हैं, जिनकी बुद्धि मंद है तो वे भी तो स्वरूप में स्थित हैं। अरे, क्या नारायण साक्षात् परमात्मा भी स्वरूप से अलग होते हैं। उनको प्रयास की क्या जरूरत होती है? क्या उनको भी मै नारायण हूँ, परमात्मा हूँ ऐसा स्मरण करना होता है? तुम सदैव बिना प्रयास ही स्वरूपस्थ हो, जायत अवस्था में स्वरूपस्थ होकर व्यवहारिक जगत का पालन करते हो, स्वप्नावस्था में स्वरूपस्थ होकर स्वप्न का अनुभव करते हो और सुषुप्ति में स्वरूपस्थ होकर सोते हो। गमी, खुशी, सोना, सपना देखना आदि सभी काम स्वरुपस्थिति में ही करते हो। कोई नई चीज नहीं बताई जा रही है। जहाँ पहुँचना है वहीं खड़ा हूँ। जिसे देखना है उसे ह देख रहा हूँ। यह मस्तों के लतीफे हैं।
अब कसर कहाँ पर रहती है। बस 'अरे' निकालना है। ये भारी पहाड़ है, क्योकि सब कुछ समझने पर भी एक तो विश्वास नहीं होता। फिर भी शास्त्रों का प्रमाण दिया जा रहा है परन्तु, परन्तु है। अनादिकालीन अभ्यास के कारण समझ में नहीं आता। यदि, सोचने लगो कि आत्मानन्द प्राप्त करना साधन का विषय नहीं है तो यों ही कैसे हमको प्राप्त होगा या यों ही कैसे प्राप्त हो गया, इतना कठिन तत्त्व बिना प्रयास के यूँ ही कैसे मिलेगा या मिल गया। बस, इतनी शंका करने से ही जहाँ से चले थे वहीं आ गये।
मुह्यन्ति यद्वत्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम् ।।
(भागवत् 7/5/13)
भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ।।
(रामायण बाल.)
अभी परसों-नरसों की बात है किसी जिज्ञासू ने कहा- स्वामी जी! आपने तो इतनी तपस्या की है, तब बोध हुआ है और हम लोग तो कुछ किये नहीं हैं। भैया ऐसा न समझो। यह तो अपना-अपना भाग्य है। एकता के कारण कभी-कभी हम बता देते हैं कि हमने यहाँ यहाँ तपस्या की, हिमालय में इतने दिन रहे, अमरकंटक में तपस्या किये आदि। एकता के कारण हम छुपा कर नहीं रखते। हमने तो कुछ नहीं किया, ऐसा न कहना, नहीं तो जहाँ से चले थे वहीं आ जाओगे। कोई-कोई जिंदगी भर कमाते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता और कोई मकान बनाते-बनाते नींव में धन का हण्डा पा जाते हैं। इसके चक्कर में तुम मत पड़ो। बड़ी विचित्र बात है, शंका करते ही सब किया कराया चौपटा 'अरे' भर न आने पाये। आया तो सब किया कराया बंटाढार हो जायेगा। जो है सो है, जैसे हो वैसे ही रहो। बनो कुछ न, यह विकल्प उठाते ही क्यों हो, जबकि तुम सनातन ब्रह्म हो। क्या भगवान भी कभी ऐसा विकल्प करता है कि भैया हम कैसे भगवान, हमने तो कुछ किया कराया नहीं। यदि कुछ करने से कोई भगवान होता है तो वह भगवान नहीं है। भगवान का यही महत्व है कि बिना कुछ किये ही भगवान है। व्यवहारिक जगत् की बात है। क्या बड़ा आदमी कुछ करता है। उसके गद्दी में बैठे-बैठे ही कार्य होता रहता है। तो फिर 'मैं' सच्चिदानन्द भगवान आत्मा हूँ। मेरी महत्ता का कोई अन्त नहीं है। जब तुम स्वयं स्वतः सिद्ध, स्वतः स्वरूपस्थ हो तो फिर अपने आपको टेटकू-खचेडू क्यों मानते हो। श्रुति कहती है-
जाग्रन निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ।
(उपनिषद)
यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।
अनिंगन मनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ।।|
(गौ.पा.का. अद्वैत प्र. 48)
जिस समय चित्त का लय न हो और चित्त विक्षप्त न हो, दोनों से रहित जो अवस्था है, 'अनिंगन् मना भासं तदा तत् काले निष्पन्न तद् ब्रह्म' अर्थात जिस समय चित्त का लय न हो और चित्त विक्षिप्त न हो, क्योंकि लय, विक्षेप से रहित अवस्था ही स्वरूपस्थिति हैं। सभी जीवधारी गाय-बैल, कूकर-सूकर सभी स्वरूपस्थ हैं। भगवान की यही तो युक्ति है। काल्पनिक संसार में जो व्यक्त करना पड़ता है।
जब अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी वृत्ति स्मरणाकार होगी या युद्धाकार, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। विषय गहन आ गया है, इसको दूसरी तरह से समझायेंगे। तुम यह ध्यान ही क्यों देते हो कि हमें स्मरण करना है। तुम तो ऐसा समझो कि स्मरण देश में स्मरण है, स्वरूप देश में स्मरण नहीं है। सब भगवत् स्वरूप ही है और यही आत्मचिंतन है। जहाँ 'अरे' आया कि मन आ गया। बस, 'अरे' निकालना है। बाकी चीज सब बनी बनाई है। कहीं प्रचण्ड वायु से आकाश भी कभी विक्षिप्त होता है, इसी तरह तुम अपने स्वरूप में रहो। जब तुम स्वरूपस्थ होने के लिए साधन करते हो, कोशिश करते हो तो लाखों जिंदगी व्यतीत हो जाती है, परन्तु फिर भी वहीं के वहीं। जब तुम चौबीस घंटे समाधिस्थ हो, सारा चराचर समाधिस्थ है, इतने पर भी तुम साधन करते हो, आश्चर्य है!!! और क्या कहें? अभी हमको देख रहे हो तो प अपने आप में देख रहे हो और अपने आपसे देख रहे हो, तब देखना कहाँ और सुनना कहाँ है। जब स्वरूप स्थान से देखो तब क्या वास्तव में कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो, भगवान का स्मरण मन से नहीं होता, मन से स्मरण अ तो माया का होता है। सब चिंतन कठिन है। इसमें कल्पना करनी पड़ती है, क परन्तु भगवान के चिंतन में कल्पना की जरूरत नहीं है, वह अपने आप है बना बनाया है। सबसे सरल है आत्म चिंतन। किसी प्रकार का चिंतन न करना ही आत्म चिंतन है। मेरा स्मरण भी कर और प्रवचन भी सुन, घर में झगड़ा हो तो झगड़ा भी कर और स्मरण भी कर, दुकान का काम भी कर और मेरा स्मरण भी कर, यह सब साथ-साथ ही होना चाहिए। यह सब वैसा ही होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। इस स्थिति में जो कुछ काम होता है वह स्वरूप से भिन्न नहीं है। भिन्न सोचोगे तो कार्य में विधि-निषेध हो जायेगा। भगवान का समत्वयोग है।
सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि ।।
(गीता 2/38)
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् ।।
(गीता 8/7)
सहजावस्था, सहजसमाधि, सहजानन्द, परम समाधि ये इसके पर्याय हैं।
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ।
भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥
(भागवत 2/9 / 36 )
समाधि चाहे निर्विकल्प हो या सविकल्प, यह कृत्रिम है, मन की है। चित्त की स्थिरता से राग नहीं और चित्त की चंचलता से द्वेष नहीं, इसी का नाम परम समाधि है और यही भगवान का सतत् चिंतन है। यदि चित्त के लिए डण्डा लेकर दौड़ते हो तो अपनी महत्ता खोकर ही करते हो। यदि लहर के पीछे सागर दौड़ता है तो सागर की महत्ता नष्ट हो जाती है। जब लहर का पता लगाओगे तब मालूम होगा कि सागर में ही उसकी उछलकूद है। इसी तरह यदि मन के पीछे साधन रूपी डण्डा लेकर दौड़ते हो तो अपनी महत्ता से दूर होते हो और इसी प्रकार वस्तुतः मन रूपी लहर की उछलकूद मुझ आत्म-सागर में ही होती है। यदि मन का विकल्प है तो उसे रोकने का साधन करो और जब 'मैं' ही है तो साधन कहाँ, बड़ी विचित्र बात है। इसकी सरलता ही कठिनाई है। धन संग्रह करना कितना कठिन है, दुकान करो, नफा उठाओ, नुकसान उठाओ तब धन संग्रह होता है, परन्तु लोग इसे कठिन नहीं मानते। आत्मपद यदि कठिन होता तो साधन गम्य हो जाता। आत्मपद तो स्वतः सिद्ध है, तुम्हें कुछ करना-धरना नहीं है, तो इसे कहते हैं कठिन। इसकी सरलता ही कठिनाई है। यदि कठिन होता तो कठिन नहीं मानते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च' इसी को परम् समाधि कहते हैं।
भगवान कहते हैं -
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ।
भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥
(भगवान् 2/9/36)
पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तयेदोंकारमात्रं सचराचरं जगत् ।
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यतेज्ञान वशान्न बोधतः ॥
(अ.रा. रामगीता 48)
अपने स्वरूप करके इसमें स्थित हो जाओ। परम समाधि के लिए साधन नहीं है। निर्विकल्प समाधि तक साधन है। महात्मा लोग लखा देते हैं। उपनिषद कहती है -
दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्व दर्शनम् ।
दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां बिना ।।
(तेजबिन्दु उप. 2/8)
तो ये चीज बनी-बनाई स्वतः सिद्ध है। 'तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च-इस स्थिति में स्थित होकर सब कार्य सहज भाव से करें तो फिर क्या अभ्यास में बैठने में कठिनाई होगी, क्या विक्षेप उठेगा।' भगवान कहते हैं कि- स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। इसी तरह मन में विक्षेप भी उठने दे और स्मरण भी कर, अगर युद्ध भी करना और स्मरण भी करना है तो फिर अब क्या चू-चपड़ है, कोई मीन-मेख नहीं रहा। विक्षेप अपना काम करे और तू अपना काम करा खूब समझ लो, अब यहाँ यदि कसर रह गई तो फिर निकलने वाली नहीं है। जितनी कसर है निकाल दो, कुछ न रहे। अरे यार! यह तो यारों के फैल हैं, तुमको यार के फैलों से क्या मतलब, यार के याराने से मतलब है। बड़ा आदमी कभी सामने सड़क से निकलता है तो पास-पड़ोस के दुकानदार देखते हैं कि कौन जा रहा है, श्रीमान् होंगे। उत्कण्ठा करते हैं, परन्तु वह बड़ा आदमी सीधे निगाह किये आगे बढ़ जाता है, उसका यही बड़प्पन है। यदि वह दोनों तरफ चकमक-चकमक देखे तो क्या वह बड़ा आदमी है। वह क्यों देखेगा, तो तुम इतने बड़े महान होकर कल्पना को क्यों देखते हो, शरीर को क्यों देखते हो, मन बुद्धि को क्यों देखते हो, इसलिए जैसे स्वभाव में हो, वैसे ही बैठे रहो। और कल्पना उठती है तो ध्यान ही क्यों देते हो। इन कल्पनाओं का क्या, इनको उठना है उठने दो, इधर-उधर देखते हैं तो देखने दो। जिसको देखना हो देखो। जो 'मैं' को देखेगा, वह मैं ही हो जायेगा। विक्षेप का नाम ही न रहेगा। इस स्थिति में रात भर बैठे रहो, मजाल है कोई विक्षेप उठे। ये लतीफे हैं छोटे- छोटे। एक पकड़ गया तो बेड़ा पार है। अभी तक विक्षेप रोकने का अभ्यास करते थे, अब विक्षेप न रोकने का अभ्यास करो। अभी तक जो अभ्यास किया है विक्षेप मानकर अभ्यास किया है और यही अभ्यास तुम्हें दुःख दे रहा है तो अब उलट दो, विक्षेप है ही नहीं इसका अभ्यास करो। भैया, यह जो बताया जा रहा है यही प्रेम का स्वरूप है। विधि-निषेध निम्न कोटि की बात है। यहाँ विधि-निषेध नहीं, जीव नहीं, ब्रह्म नहीं, यहाँ तो सब भावों का अभाव है। हमारी तरफ देखना, जैसे बैठे हो, बैठे रहो, विक्षेप उठते हैं तो उपेक्षा करो। जब तुम उनकी तरफ देखोगे तो वे अकड़ जायेंगे। अब तुम न देखने की कोशिश करो और यदि दिखता है तब भी उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब देखता हूँ तब दिखता है और यदि दिखता है तो 'मैं' ही दिखता हूँ। जब विक्षेप को देखता हूँ तब विक्षेप दिखता है और न देखूँ तो न दिखे। किसी प्रकार समझ लो। अपने मन, बुद्धि को मुझमें लगा दो। जो भी नाम रूप सामने आये 'मैं' का डण्डा लगा दो, 'मैं' हूँ। जहाँ तुमने 'मैं' हूँ कहा तो मन भगवान में अर्पित हो गया। यही मन को, बुद्धि को भगवान में अर्पित करना है। मन, बुद्धि की तरफ किंचित् मात्र भी न देखना, यही भगवान का चिंतन है। जब मन बुराई, भलाई की तरफ नहीं देखता, सारे प्रपंच की तरफ नहीं देखता, 'मैं' को छोड़कर दूसरी चीज की तरफ नहीं देखता, तब मन ही भगवान है। यह सूत्र पकड़ लेना, चाहे और सब भूल जाना। एक विचित्र बात और आ गयी, इसे भी बता दें। तुमसे कोई पूछे कि भगवान कहाँ है तो तुम डंके की चोट पर कह देना कि जहाँ 'मैं' हूँ और जब पूछे भगवान कौन है ' तो कहना जो 'मैं हूँ। और जब पूछे 'मैं' कौन हूँ तो कहना जो भगवान है। और ना 'मैं' कहाँ हूँ, जहाँ भगवान है। भगवान का क्या लक्षण है-जो अपने आप 'मैं' आत्मा के सिवाय दूसरे को नहीं देखता वही भगवान है। कितनी सुंदर * व्याख्या है? जो में को ही देखता है, मैं को ही सुनता है, मैं को ही जानता है, वही सुख स्वरूप भूमा पद है। यही नारायण पद है और यही आत्म पद है।
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ।
यत्र अन्यत्पश्यति अन्यच्छृणोति अन्यद्विजानाति तदल्पं ।
यो वै भूमा तत् सुखं यदल्पं तद्दुःखम् ॥
(छा.उ..7 / 24 / 1)
जो दूसरों को देखता है, जो दूसरे को सुनता है, वह अल्प है और दुःख रूप है और 'योवै भूमा तत् सुखम्' यह भगवान के चिंतन का कितना सुन्दर अभ्यास है। विक्षेप को देखते हो, उस पर ध्यान देते हो तो जीव बन जाते हो और नहीं देखते हो तो भगवान बने बनाये हो। स्वतः सिद्ध है।
संशान्त सर्व संकल्पा या शिलावदवस्थितिः ।
जायन निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥
सारे व्यवहार स्वरूप स्थिति में ही हो रहे हैं। कल्पनाएँ, भावनाएँ, अच्छे- बुरे विचार भी उठ रहे हैं, यही तो विक्षेप है और ये विक्षेप तुम स्वरूप स्थिति में देख रहे हो। फिर डण्डा लेकर विक्षेप को मारने के लिए क्यों दौड़ रहे हो। विक्षेप को मारने बैठे हो कि भगवान का ध्यान करने। शहंशाह बैठा है तख्त पर, मच्छर-खटमल आते हैं, आने दो। वे क्या कर लेंगे? वे कर ही क्या सकते हैं। सब कुछ बता दिया, अब भूलना नहीं और यदि कदाचित् भूलोगे भी तो भूलने वाले को भी वहीं भूल जाओगे।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैष्यस्य संशयम् ।।
(गीता 8/3)
टेप रिकॉर्डिंग द्वारा श्रुत प्रवचन का संक्षिप्त रूप (रायपुर 1963)
4.इदं शरीरं कौन्तेय
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोनिं यतज्ज्ञानं मतं मम् ।।
(गीता 13/1/2)
शरीर है क्षेत्र और इस शरीर को जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर का चैतन्य तत्व है आत्मा और वह क्षेत्रज्ञ आत्मा 'मैं' हूँ। आत्मा के अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं, वे सब संघात हैं। जितने भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, वे सब संघात कहे जाते हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। यह प्रक्रिया है।
सबसे पहले यह समझ लो कि जो कुछ भी संसार में भास रहा है भूत, भौतिक प्रपंच दिख रहा है, यह सभी पंच भौतिक हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इनको पंच महाभूत कहते हैं। सारा संसार इन पंच महाभूतों का खेल है। यह शरीर जो दिख रहा है यह स्थूल शरीर है। इसका एक- एक तत्व पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सबका आपस में पंचीकरण होता है और एक-एक तत्व से पाँच-पाँच तन्मात्राएँ उनके विषय आदि होते हैं। इसलिए पाँच पंजे पच्चीस हुए। इन पच्चीस तत्वों से, इनके पंचीकरण से, यह स्थूल शरीर बना है। इसलिए यह शरीर न 'मैं' हूँ और न यह शरीर मेरा है। यह पंच भूतों का विकार है। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। शरीर ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ। शरीर असत्य है, मैं सत्य हूँ। शरीर प्रपंच है, मिथ्या है, दुःख रूप है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, स्वप्न है और 'मैं' आत्मा चेतन हूँ। यह शरीर न मैं हूँ और न यह मेरा है। जब यह शरीर 'मैं' नहीं और मेरा नहीं तब केवल शरीर से संबंध रहने के कारण ही मैं कहता हूँ कि यह शरीर मेरा है। मेरा कहने से ही यह सम्बोधित होता है कि यह मैं नहीं हूँ। मेरा मकान कहने से ही यह मालूम होता है कि मकान मेरा है, मैं मकान नहीं हूँ। कहते हो न, मेरी नाक, मेरी आँख, मेरा पाँव, मेरा शरीरा स्वाभाविक सभी लोगों के मुँह से ऐसा निकलता है। और विचार करके देखो तो यह मेरा भी नहीं है। शरीर पंच न निकला है, पंच भूतों से बना हुआ है। मकान जैसे ईंट गारों से बनता है। ही माँस-मज्जा से यह शरीर बनता है। हड्डी आदि यह सब इस मकहर ही माँ है। जैसे मकान में खिड़कियाँ होती है, दरवाजे होते हैं वैसे ही च शरीर के नौ दरवाजे हैं। जैसे घरों में घास-फूस उग आते हैं वैसे ही देह शाल हैं। कोई मकान लाल मिट्टी, कोई सफेद, कोई काला, पीला रंग ह होता है, रंगा जाता है। ऐसे ही कोई काला, कोई गोरा, कोई सांवला रहने की गरज से मेरा मकान कहता हूँ। यह मकान पंच भूतों का है। इस अन्दर 'मैं' हूँ जरूर, पर यह 'मैं' नहीं हूँ। यह हुआ स्थूल शरीरा परमात्मा और अपने आप में भेद का जो भ्रम है, यह सब देहाध्यास के कारण है। ज तक साढ़े तीन हाथ की खुदी है, तब तक खुदा दूर है और जब यह देहाध्यास- गया, तब फिर खुदा ही खुदा है। खूब समझ लो, यह शरीर उत्पत्ति-विना वाला है, घटने-बढ़ने वाला है। इसको संघात कहते हैं, नाशवान कहते है
देहात्म बुद्धिजं पापं न तद् गोवध कोटिभिः ।
आत्माऽहं बुद्धिजं पुण्यं न भूतं न भविष्यति ॥
यदि शास्त्रों पर विश्वास है तो अपने आपको जो देह मानता है उसे एक करोड़ गौ हत्या का पाप लगता है और जो अपने-आपको आत्मा 'मैं' हूँ ऐसे जानता है, इससे अधिक पुण्य भी नहीं होता है। इसलिए जान लो कि यह स्थूल शरीर न 'मैं' हूँ और न यह मेरा है।
अब एक शरीर इसके अंदर है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वह भी पंच तत्वों से बना हुआ है, परन्तु उनका पंचीकरण नहीं हुआ है, यह अपंचीकृत है। 19 तत्वों का बना है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण और चतुष्टय अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसी के सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, यम-यातना शरीर, अष्टकापुरी, अन्तःवाहक पर्याय नाम हैं। इस स्थूल शरीर का जन्म कब हुआ, संभवतः कब तक यह रहेगा यह तो जाना जाता है, परन्तु सूक्ष्म शरीर तो अनादिकाल का है, इसकी जन्म कुण्डली नहीं है। जब से अज्ञान पैदा हुआ तब से सूक्ष्म शरीर पैदा हुआ। सूक्ष्म शरीर अनादि है, परन्तु अनन्त नहीं है, सांत है। कब पैदा हुआ? जिस दिन अज्ञान पैदा हुआ। जब तक अज्ञान का नाश न होगा बराबर तारतम्य लगा रहेगा। जिस दिन अज्ञान का नाश होगा, उसी दिन सूक्ष्म शरीर का भी नाश होगा, आना- जाना बंद होगा? इसी को मोक्ष कहते हैं। सूक्ष्म शरीर ही आता-जाता है,एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और पुण्य-पाप भोगने के लिए, अपने प्रारब्ध का फल भोगने के लिए , सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर का ढाँचा धारण करता है। मुझ आत्मा से इसका कोई संबंध, लेना-देना नहीं है- ऐसा समझो।
पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय जो स्थूल शरीर में देख रहे हो-आँख, कान, नाक ये सब इन्द्रिय नहीं है। यह इन इन्द्रियों के अनुभव का साधन है। इनके विषयों को ग्रहण करने का साधन हैं। आँख देखने का साधन है। कान सुनने का साधन है। नाक सूंघने का साधन है। इन्द्रियाँ भीतर हैं और सूक्ष्म हैं। नाक, कान, आँख के अंदर हैं, वह दिखती नहीं हैं। फिर पंच प्राण है, प्राण का स्थान है हृदय। इसकी क्या क्रिया है? 21600 श्वांस को बाहर- भीतर प्रतिदिन ले जाना होता है। मनुष्य के श्वांस का प्रमाण है कि 15 श्वांस 1 मिनट में वह लेता है, घड़ी लगाकर देख लो। प्राण वायु का काम है 900 श्वांस प्रति घंटा और 21600 श्वांस 24 घंटे में भीतर-बाहर करना। 73 लाख 77 हजार श्वासें 1 साल में होती हैं और यदि मनुष्य 100 साल तक जीवित रहे तो 93 करोड़ 31 लाख 20 हजार श्वासें लेगा। शरीर में साढ़े तीन करोड़ छेद हैं। हमारे ऋषियों ने कुछ बाकी नहीं रखा है, सब बताये हैं। यह तो चलनी से भी बढ़कर है। भूख-प्यास प्राण को लगती है। श्वांस-प्रश्वांस निकलता जाता है और हृदय उसका स्थान है। 'उदान' कण्ठ में रहता है, डकार पैदा करता है। 'हिता' नाम की नाड़ी बाल से भी महीन होती है, कण्ठ में है, उसमें स्वप्न पैदा होता है। 'समान' वायु नाभि में रहता है। यह सब रसों को श्वांस रूपी धोंकनी से शुद्ध कर 72 नालियों से शरीर रूपी बगीचे को बतौर माली सींचता है। बागवान का काम करता है। 'व्यान' वायु संधियों को मोड़ता है। 'अपान' वायु स्वीपर का काम करता है। शरीर की गंदगी को हटाता है, नहीं तो गंदगी फैल जायेगी। मल-मूत्र को निकालता है, परन्तु 'मैं' आत्मा देखता रहता हूँ। इन प्राणों से मेरा कोई मतलब नहीं है। 'मैं' ब्रह्म आत्मा अकर्त्ता हूँ। 'मैं' द्रष्टा हूँ, ज्ञाता हूँ, साक्षी हूँ। अब पंच वायु और होते हैं। सुनो- 'नाग' डकार पैदा करती है। 'कूर्म' आँख को मूंदती और खोलती है। 'कृकिल' छींक पैदा करती है। 'देवदत्त' जंभाई पैदा करती है और 'धनंजय' मुर्दा शरीर में भी रहता है। इसी से ज्यादा दिन में मुर्दा फूल जाता है। यदि वायु न रहे तो फूलेगा कैसे? जब जलाया जाता है, तब अपने कारण में लीन हो जाता है, परन्तु मैं आत्मा इसका साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ज्ञाता हूँ, अकर्त्ता हूँ।
इस शरीर के अंदर पंच कोष हैं- अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनन्दमया कोष का अर्थ होता है म्यान और खजाना। शरीर रूपी म्यान (कोष) में आत्मा रुपी तलवार है अथवा आत्मा रूपी धन शरीर रूपी खजाने (कोष) में है, यह हुआ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ।
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मन रूपी राजा की पटरानी हैं और पंच कर्मेन्द्रियाँ इन ज्ञानेन्द्रियों की बांदी हैं। इनके पाँच विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एक-दूसरे के लिए सेवा करती हैं।
अलि पतंग मृग मीन गज जरें एक ही आँच ।
तुलसी वे कैसे जिये जिनको लागे पाँच ।।
अलि (भौरा), पतंग (पंखी), मीन (मछली), गज (हाथी) ये सब एक-एक विषय में मारे जाते हैं। भौरा गंध विषय में मारा जाता है। भौरा कमल के फूलों में इतना उन्मत्त हो जाता है कि वह कमल के भीतर पराग के गंध में मस्त रहता है। शाम होते ही उसको निकल जाना चाहिए, परन्तु वहीं पड़ा रहता है। शाम हो जाती है और कमल का फूल संपुटित हो जाता है। भौरा वहीं फँस जाता है, तब वह सोचता है कि-अब तो फँस गया। जब सुबह होगी तब सूर्य भगवान उदय होंगे, कमल के फूल खिलेंगे और भाग जाऊँगा। रात्रि तो व्यतीत हो गयी, परन्तु अरुणोदय के पहले ही एक प्यासा हाथी जंगल से निकला और धमाके से तालाब में कूद पड़ा। उसने पेट भर पानी पिया और कमल, कमल के पत्ते, नाल सब सूँड से लपेट कर भोजन कर गया। इस प्रकार गंध विषय में भौरा मारा गया। रूप विषय में पतंगे नाच-कूद कर नष्ट हो जाते हैं। मृग शब्द विषय में मारा जाता है। शिकारी जंगल में मृग फँसाने जाता है, तब बाँसुरी बजाता है और 'मृग-नाद' को सुनकर मृग एक चित्त हो जाता है और शिकारी के चंगुल में फँस जाता है। हाथी स्पर्श विषय में मारा जाता है। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पास ये पाँचों विषय भोग के साधन हैं, उनका क्या हाल होगा?
आँख के देवता है सूर्य, इसका क्या प्रमाण है? बर्फीली जगह में इसका पता लगता है, जहाँ सब अंग तो गल जायेंगे, परन्तु आँख को ठण्डक न लगेगी। क्यों न ऐसा हो, भगवान सूर्य का जो निवास स्थान है। जिह्वा (रसना) इसमें वरुण देव का निवास है। यह कभी नहीं सूखती। मुँह यह अग्नि देवता का स्थान है। पानी मुँह में लेकर थोड़ी देर में बाहर करो तो कुनकुना हो जावेगा। कान का दिशा, नाक का अश्विनी कुमार, हाथ का इन्द्र, पैर का उपेन्द्र देवता है। पैर क्यों पड़ते हैं, सिर क्यों नहीं पड़ते? सिर तो पैर से पवित्र होता ही है, फिर क्यों चरण छूते हैं। लोग कहते हैं-चरण हुई महाराज, पाँव पड़ी महाराज। यह इसलिए कि पैर में भगवान 'उपेन्द्र' का निवास है, 'उपेन्द्र' वामन भगवान का नाम है। विष्णु स्वरूप है। इसलिए चरण पूजन का अर्थ भगवान विष्णु का पूजन करना है। मन का चन्द्रमा, हृदय का नारायण, अन्तःकरण का विष्णु, शिश्न का प्रजापति, गुदा का यम, बुद्धि का बह्मा, अहंकार का रुद्र, देवता हैं।
इन्द्रिय सुरन्ह न ग्यान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई ।।
(रामायण उत्तर.)
देवता बड़े विषयी होते हैं, विषय की रुचि इनमें सदैव रहती है। ये बड़े चालाक होते हैं। वृद्धावस्था में जब शरीर निर्बल हो जाता है, तब एक-एक करके सभी स्थान छोड़ जाते हैं। फिर कान से सुनाई नहीं पड़ता। आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। देवता क्या करेंगे रहकर, इन्द्रियाँ तो शिथिल हो रही हैं। इन्हीं से विषय भोग हो सकता है, फिर रहकर क्या करेंगे? बस, सब चले जाते हैं, स्वार्थी जो हैं।
शंका है- 'शरीर की मृत्यु हो जाने पर आत्मा निकलती है या प्राण निकलता है?' क्या कहा जाय? यह भी समझो, व्यापक चीज का आना- जाना नहीं होता। आत्मा का आवागमन नहीं है। फिर, ऐसा कौन-सा तत्व है, जिसके निकल जाने से 'राम-नाम सत्य है' कहने लगते हैं। सुनो-इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है। सूक्ष्म शरीर ही एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। अब प्रश्न होता है कि सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जाता है कि नहीं। हाँ जाता है, परन्तु ऐसा नहीं जैसे घोड़े पर बैठकर सवार जाये। तब फिर किस प्रकार जाता है। समझो (स्वामी जी अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ संकेत करते हैं) इसको कहते हैं घड़ी, उदाहरण देकर समझा रहे हैं। इसका बाल कमानी, कांटे, घंटे के कांटे, मिनट के कांटे, सेकण्ड के कांटे और सारे पुर्जे लोहे के बने हैं, लोहा इसके अन्दर व्यापक है। अब इस घड़ी का प्राण वायु क्या है? बाल कमानी। वह भी लोहे की बनी है। यदि, इस घड़ी की बाल कमानी निकाल कर दूसरी घड़ी में लगा दी जाय तो इस घड़ी का टिक-टिक व्यापार बंद हो जायेगा और दूसरी घड़ी जिंदा हो जायेगी। तब लोहा निकला कि बाल कमानी? बाल कमानी निकली और बाल-कमानी के साथ लोहा गया कि नहीं? हो गया, परन्तु कारण रूप से गया। इसी तरह शरीर घड़ी है, सूक्ष्म शरीर बाल कमानी पंच प्राणवायु, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेन्द्रियाँ, चतुष्टय अन्तःकरण, पंच कोश, सत् रज तम, जागत स्वप्न सुषुप्ति ये सब प्रपंच है और ये सब आत्मा रुपी लोहे से बने हुए हैं। आत्मा ठसाठस भरा है। सूक्ष्म शरीर के साथ आटमा रुया कि नहीं? हाँ गया, परन्तु अभिन्न होकर गया। कारण रूप से गाया इस तरह आत्मा का आना-जाना मानना चाहिए। अलग होकर नहीं जाया। आरमा आप्त (च्याप्तौ) धातु से बनता है। आत्मा लबालब है। तिल भर भी जगह खाली नहीं है, व्यापक है। आत्मा कहीं से न आता है और न कही जाता है।
जब सो जाते हो तब सूक्ष्म शरीर से स्वप्नावस्था में स्वप्न देखते हो। गाढ़ी नींद में सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, कारण शरीर ही रहता है। उस अवस्था को अज्ञान-अवस्था कहते हैं और कारण शरीर की संज्ञा देते हैं। कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल शरीर होता है। जब गाढ़ी नींद से उठे तो कहते हो 'आज मुझे खूब अच्छी नींद आयी, तबियत मस्त हो गयी, बड़ा आनन्द आया। कुछ पता ही नहीं रहा।' इस गाढ़ी नींद का पता तुम सबेरे उठकर देते हो। तब भैया 'नहीं पता' का पता किसको रहता है, यही अज्ञान है। आत्मा इन तीनों शरीर से परे है। सच्चिदानन्द व्यापक तत्व 'मैं' हूँ। न 'मैं' स्थूल शरीर, न 'मैं' सूक्ष्म शरीर और न 'मैं' कारण शरीर हूँ। 'मैं' इनका अनुभव करता हूँ, इनका आधार हूँ. इनका ज्ञाता हूँ। 'मैं' आत्मा का नाश नहीं होता है, परन्तु अज्ञानवशात् वह अपने आपको मान लेता है संसारी जीव, साढ़े तीन हाथ का शरीर और अनादिकाल से भटकने का यही कारण 1 है। बस, जहाँ अपने आपको जीव माना, मन पैदा हो गया, प्रपंच पैदा हो 1 गया। फिर तो असाध्य रोग हो जाता है।
इतनी महान भूल !! स्वयं सच्चिदानन्द होते हुए भी अपने को क्या मान 1 लिया है। इस विषय में कर्ण का आख्यान बताते हैं -
महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब भी अर्जुन कर्ण के सामने आता तो बाणों । की वर्षा के साथ-साथ जोर से पुकार कर कहता- 'अरे दासी पुत्र शूद्र! तू क्या लड़ेगा?' इससे कर्ण के मन में ग्लानि पैदा हो जाती और वह अपने को हेय समझता। यद्यपि कर्ण सूर्य भगवान का पुत्र था, परन्तु बचपन से दासी ने पाला था। दुर्योधन के यहाँ पला था इसलिए अपने को दासी पुत्र ही मानता था। उसको अपने क्षत्रिय शरीर का ज्ञान न था। अपने पैदाइश की कथा उसे ज्ञात नहीं थी। जब भी अर्जुन की ललकार सुनता कि 'अरे दासी पुत्र।' तब उसका हृदय कमजोर हो जाता था। एक दिन इसी विषय के उधेड़बुन में हृदय व्यथित हो गया, उसका चित्त द्रवित हो गया। वह रो रहा था। इसी समय भगवान नारद वहाँ पहुँचे और कर्ण को सम्बोधन करके पूछा कि 'बेटा तू क्यों रो रहा है?' कर्ण ने बताया कि 'महाभारत में अर्जुन मुझे दासी पुत्र कहता है। मैं क्या करूँ। दासी ने मुझे पाला है। मुझे अपनी उत्पत्ति का पता नहीं, मेरे माता-पिता कौन हैं?' नारद जी को दया आ गयी। वे बोले 'बेटा तू गलत धारणा छोड़ दे, तेरी माता वही है जो अर्जुन की माता है। तू भी कौन्तेय है, सुन तेरी उत्पत्ति की कथा ऐसे है-एक समय महर्षि दुर्वासा भिक्षा लेने आये थे। उस समय तेरी माता कुन्ती सुन्दरी कुमारी थी। वह दुर्वासा ऋषि को भिक्षा देने आयी। जब कुन्ती भिक्षा दे रही थी तब दुर्वासा ऋषि को मन में बड़ा संताप हुआ। वे बोले कि बेटी तेरे सुन्दर स्वरूप को देखकर दुःख होता है। भविष्य में जो तुझे पति मिलेगा, वह पाण्डु रोगी होगा। मैं तुम्हें एक आकर्षण मंत्र देता हूँ। जब तुझे संतान की इच्छा हो, इस मंत्र से तू जिस देवता का आकर्षण करेगी वे देवता तेरे पास आयेंगे। यह मंत्र तू अपने पति की आज्ञा लेकर उपयोग में लाना।' दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद देकर चले गये। एक दिन तुम्हारी माता ने जब वह क्वाँरी ही थी, इस आकर्षण मंत्र का उपयोग सूर्य भगवान के प्रति कर दिया। वह मंत्र का प्रभाव देखना चाहती थी। जब आकर्षण कर दिया तो सूर्य भगवान प्रकट हो गये और बोले कि देवी तेरी इच्छा पूर्ण हो। कुन्ती घबरा गई और रोने लगी। सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा आना तो व्यर्थ न होगा। उसने (कुन्ती ने) सूर्य के वीर्य को दोने में लेकर नदी में प्रवाहित कर दिया। उसे मछली निकल गयी। केंवट ने जब उस मछली को पकड़ा उस समय उसके कान से तुम निकले। और दासी ने दुर्योधन के यहाँ तुम्हें पाला। वस्तुतः, तू दासी पुत्र नहीं है। नारद के कहने पर कर्ण ने माता कुन्ती के पास जाकर पूछा। कुन्ती ने भी यही बात बतायी, तब भ्रम निकल गया। फिर जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने ललकारा कि 'अरे दासी पुत्र!' 'मूर्ख तू क्या जानता है। मैं सूर्य भगवान का पुत्र हूँ। जब जोर से कर्ण ने ललकारा तब अर्जुन को मालूम पड़ा कि कोई है। कहने का मतलब यह है कि आप स्वयं साक्षात् चैतन्य ब्रहा होकर अपने आपको क्या का क्या मान बैठे हैं, मैं संसारी जीव हूँ। टेटकू-खचेड बना फिरता है। समझो एक दृष्टांत है इस पर -
" एक गड़रिया था। जंगल में भेड़ चराया करता था। किसी दिन हाल ही में पैदा हुआ सिंह का बच्चा उसे जंगल में मिल गया। गड़रिया सिंह के बच्चे को भेड़ा का दूध पिलाता और भेड़ों के साथ ही रखता था। उसका नाम भी भेड जजैसा रख दिया। कुछ दिन बीतने पर सिंह शावक भेड़ों में इतना मिल गया । कि वह मानने लगा कि मैं भी भेड़ हूँ। उनके ही समान चलना, आवाज लगाना। आदि व्यवहार करने लगा। एक समय जब यह सिंह बालक भेड़ों के साथ चर रह था तो उधर से जंगली सिंह निकला। उस सिंहशावक को देखकर जंगली सिंह आश्चर्य करने लगा कि यह सिंह होते हुए भी भेड़ों के साथ कैसे रह रहा है? उसने जोर से दहाड़ा। दहाड़ सुनकर सभी भेड़ भागे। वह पालतू सिंह भी भेड़ों के साथ भागा। तब जंगली सिंह ने पुकारा 'ओ मेरे जाति वाले, जरा खड़ा रह, तेरे से मुझे कुछ बात करनी है।' उस पालतू सिंह ने खड़ा होकर पूछा कि क्या बात है। जंगली सिंह ने कहा 'यार, तू सिंह होकर भेड़ों के साथ रहता है, शर्म है।'
पालतू सिंह- 'मैं सिंह नहीं हूँ, भेड़ हूँ भेड़।'
जंगली सिंह- 'तू भेड़ नहीं, देख तेरी आँखें बड़ी-बड़ी, भेड़ों की आँखें छोटी-छोटी हैं। भेड़ों की कमर मोटी तेरी कमल पतली है। तेरे दाँत बड़े-बड़े और यार तेरे शरीर का एक भी अंग भेड़ जैसा नहीं है। तू भेड़ नहीं है, सिंह है ।''
पालतू सिंह- 'क्या कहते हो, मैं बड़ा भेड़ हूँ और ये छोटे भेड़ हैं। कुछ भी कहो मैं भेड़ ही हूँ और नहीं तो प्रमाण दो।'
इस पर जंगली सिंह उसे नदी में ले गया और दोनों की परछाइयाँ मिलान कराने लगा। बोला- 'देख परछाई मिला तो सही, मिलती तो है न। मेरे कान और तेरे कान एक से हैं। तेरी पूँछ और मेरी पूँछ एक सी है। मेरे यार तू तो सिंह आ
पालतू सिंह- 'प्रमाण तो यही मिल रहा है। ऐसा तो मालूम होता है कि मैं भी सिंह हूँ, पर एक कसर है। तुम्हारी पूँछ ऊपर की ओर उठी है और मेरी पूँछ नीचे की ओर है।'
इस पर जंगली सिंह ने अपने सामने के दोनों पैर जमीन पर खूब गड़ाकर कहा- 'तू भी ऐसा कर और फिर शरीर को अपनी तरफ खींच और कमर को उचका कर ऊपर तो कर।''
जब पालतू सिंह ने वैसा ही किया तो जो कमर झुकी हुई थी, वह सीधी हो गयी और जो पूँछ दबी थी, वह ऊपर को उठ गयी। तब जंगली सिंह ने पूछा- 'अब तो कोई कसर नहीं है?'
'नहीं भैय्या, सब भ्रम निकल गया। संशय-विपर्यय निकल गये। मैं जान गया कि मैं सिंह हूँ, भेड़ नहीं।'
'तब फिर दहाड़ जोर से।'
परन्तु, पालतू सिंह दहाड़ देने के बजाय मिमियाया- 'मैं - मैं' क्या करे भाई, बोली ही भूल गए हैं। तुम बोलो तो साथ में मैं भी बोलूं।
जब सिंह दहाड़ने लगा तब पालतू सिंह भी दहाड़ने लगा।
इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि मनुष्य भेदवादी गड़रिये, साम्प्रदायिक-गुरु, आचार्यों के चक्कर में पड़कर अपने शुद्ध स्वरूप, सत्- चित्-आनन्द स्वरूप को भूलकर मानता है कि मैं संसारी जीव हूँ। यह मैंने मान लिया है कि मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, स्त्री-पुरुष हूँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यासी हूँ-पुण्यी-पापी हूँ, लम्बा-चौड़ा हूँ, काला-गोरा हूँ। अज्ञान के कारण इस प्रकार मान बैठा हूँ। जंगली सिंह के समान कोई महान पुरुष आते हैं और 'तत्त्वमसि' तथा 'अहम् ब्रह्मास्मि' इन महा-वाक्यों की जब दहाड़ देते हैं और अपने स्वरूप को वेदान्त रूपी तालाब में दिखा देते हैं, तब वे अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं, लखा देते हैं कि तू आत्मा है, शुद्ध सच्चिदानन्द है, व्यापक है, तब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मैं संसारी जीव हूँ, ऐसा मानना वास्तविकता नहीं है यह भ्रम है, अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करो। अपने आपको जानो, अपने आपको पहिचानो।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोनिं यतज्ज्ञानं मतं मम् ।।
(गीता 13/2)
हे अर्जुन! क्षेत्र जो यह शरीर है, उसका जानने वाला 'मैं' हैं। 'मैं' ही क्षेत्रज्ञ हूँ, मुझसे क्षेत्र भिद्म नहीं है। सारे चराचर में जो आत्मा है, वह आत्मा नेहा है। व्यापक तत्व आत्मा है, वह 'ग' है। अन्न प्रश्न होता है। कि जब "मैं' ही बहा हूँ तब अपने-आपको कैसे भूल गया। 'मैं' ने अपने आपको संसाध हीच्या मोना? सनातन ब्रह्मपना क्यों भूल गया? सुनो, अभी यहाँ पर सब बैठे हो इस पण्डाल में देखो, एक सांप, काला नाग, तुम्हारे ऊपर कहीं से आकर गोद में आ गिरा। उस समय क्या विचार करना चाहिए कि यह साँप कहाँ से आया या साँप को तुरन्त फेंक देना चाहिए? क्या सोचना चाहिए कि साँप का इधर आना तो हो नहीं सकता, फिर आया किधर से? ऐसे सोचने बैठोगे तो सांप काट खायेगा। कहीं से आया हो अपनी बला से। तुम्हारा कर्त्तव्य यही है कि उसे जल्दी दूर फेंक दो, तुरन्त साँप को फेंक दो। कहाँ से आया यह मत सोचो? विचार मत करो कि अज्ञान क्यों आया, कहाँ से आया? अभी मत सोचो। मुक्ता के वाक्य पर विश्वास करो। तब तुम्हें फिर मालूम करना कुछ न रहेगा, तुम जान लोगे कि जिसको 'मैं' अज्ञान (काला नाग) समझा था वह न था, न है और न आगे रहेगा। 'मैं' पहले भी ज्ञान स्वरूप था, अभी भी ज्ञान स्वरूप हूँ और आगे भी ज्ञानस्वरूप रहूँगा। मेरा अज्ञानी समझना भ्रम था। 'मैं' शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ। मुक्त स्वरूप हूँ। शास्त्रों के कहने से अज्ञान रूपी काले नाग को तुरन्त फेंकना बुद्धिमानी है। अभी यह अज्ञान कहाँ से आया यह प्रश्न हल न होगा। मुक्ता की वाणी पर विश्वास करके उसे दूर करो। फिर देखोगे कि तुम स्वयं सच्चिदानन्द आत्मा हो, अज्ञान तीन काल में है ही नहीं।
दूसरी युक्ति से भी समझो। देखो, जब मैं सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ, यहीं खड़े हो जाओ। अब इसके आगे मत जाओ और प्रश्न करो तब यह अज्ञान कहाँ से आया, जबकि 'मैं' सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ, यहीं खड़े रहो। इस स्थान से मत हटो। अब क्या अज्ञान परक प्रश्न होगा? इस स्थान को छोड़कर निम्न स्तर पर आते हो तब यह सब प्रश्न होता है। जब 'मैं' सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ, इस स्थान में अज्ञान परक प्रश्न होगा क्या? नहीं। अंधकार देश में अंधकार है, न कि प्रकाश देश में। इसी तरह अज्ञान देश में अज्ञान है न कि नारायण देश में। आत्म देश से देखोगे तो न ज्ञान है और न अज्ञान है। सूर्य देश से देखो तब सूर्य में न प्रकाश है और अंधकार है, न दिन है, न रात है, सूर्य ही सूर्य है। इसी तरह अपने स्वरूप आत्मा में देखोगे तब न अज्ञान है और न ज्ञान है। सदैव एक चेतन ही चेतन है।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
क्षेत्रक्षेत्रझयोनिं यत्तज्ज्ञानं मतं मम् ।।
(गीता 13/2)
हे अर्जुन, इस प्रकार जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, यही ज्ञान है, बतज्ज्ञानं' इसी का नाम ज्ञान है।
टेप रिकॉर्डिंग द्वारा श्रुत प्रवचन का संक्षिप्त रूप
5.ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥
(गीता 15/1)
यहाँ पर संसार, को अश्वत्थ का वृक्ष माना है। अश्वत्थ-जिसकी जड़ ऊपर को बतायी गयी है, शाखाएँ, प्रतिशाखाएँ नीचे की ओर फैली हुई है और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों जो वेद हैं ये सब पत्ते हैं। इस प्रकार के वृक्ष अश्वत्थ को जो जानता है, 'सवेद वित्' वही वेद विव् है। वहीं वेद वेत्ता है। वहीं वेद का जानने वाला है। संसार का नाम अश्वत्थ क्यों पड़ा? अश्वत्थ का अर्थ होता है- अ=न, नहीं, स्व = प्रातःकाल, स्थ = ति रहे - स्थित, इति अश्वत्था अंधकार में रहे और प्रकाश होने पर जो न रहे, उसको कहते हैं 'अश्वत्था' संसार अज्ञान के अंधकार में तो है, परन्तु ज्ञान का प्रकाश होने पर नहीं रहता। इसीलिए संसार को अश्वत्थ कहा है क्योंकि रज्जु में जो सर्प है वह अंधकार रहने तक है और अंधकार के नष्ट हो जाने पर, जब प्रकाश हो जाता है तब वह मिथ्या सर्प, नहीं रहता। वह खो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी तरह यह संसार अज्ञान के अंधकार तक ही जो है। अज्ञान ही संसार है। यावत् काल अज्ञान है, तावत्काल संसार भासता है। अज्ञान के दूर होने पर, विनाश हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर संसार का पता नहीं रहता। जिस प्रकार रज्जु का ज्ञान, अंधकार का नाश और सर्प का अभाव (विनाश) ये तीनों बातें एक ही टाइम में होती हैं, ऐसा नहीं कि अंधकार का अभी नाश हो जाय और रज्जु का परिज्ञान साल भर बाद हो और उसके बाद फिर सर्प का विनाश हो, ऐसा नहीं है, एक ही टाइम में तीनों की तीनों चीजें होती हैं। इसी तरह अनन्तकालीन अज्ञान की दशा है। कभी- कभी लोग कहते हैं कि महाराज, ज्ञान धीरे-धीरे होगा। तो सुनो-किसी पर्वत की कन्दरा में हजारों-लाखों वर्षों का अंधेरा छाया है, अंधकार है। वहाँ का अंधकार यह नहीं कहता कि हमारा यहाँ पर लाखों वर्षों का कब्जा है, हम जल्दी नहीं जायेंगे। जहाँ तुम प्रकाश लाये कि वह अंधकार कहाँ चला जाता है, इसका पता नहीं लगता। इसी तरह अनन्तकाल का अज्ञान जो हृदय में छाया है, जिस समय आत्म स्वरूप का बोध होता है, उस समय यह अनादिकाल का अज्ञान कहाँ चला जाता है, भाग जाता है, कहीं कुछ पता नहीं लगता। इसी तरह अज्ञान का नाश, स्वरूप का बोध और संसार का नाश तीनों एक ही टाइम में होते हैं।
भगवान ने इस संसार वृक्ष का नाम रखा है 'अश्वत्था' इसकी जड़ ऊपर को है। ऊपर का अर्थ होगा, सबसे परे। अरे भाई! रज्जु में जो सर्प भासता है, उस सर्प की जड़ क्या है? रज्जु। जिसमें भासता है वही उसका आधार है, जड़ है। यह अश्वत्थ संसार भास रहा है। किसमें भास रहा है? अपने स्वरूप में, अपने आप में, ऊर्ध्व, यह सबसे परे है। पंच प्राण से परे, पंच ज्ञानेन्द्रियों से परे, पंच कर्मेन्द्रियों से परे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे, वाणी से परे, दृष्टि से परे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से परे।
'ऊर्ध्व' का अर्थ होता है-जो आधार स्वरूप है, जिसकी जड़ ऊपर को है। भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सुवल, तलावल, महातल, रसातल, पाताल अनेकानेक ब्रह्माण्ड इसमें है, यह सब शाखाएँ-प्रशाखाएँ फैली हुई हैं।
ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम् ।।
अव्ययम्-अव्यय के दो अर्थ होते हैं। अव्यय-अविनाशी और अव्यय- जो कभी खत्म न हो, पूर्ण का पूर्ण रहे। यहाँ पर अव्यय का अर्थ पूर्ण का पूर्ण लगेगा, क्योंकि यह संसार का तारतम्य तो बंद होना नहीं है, लगा ही रहेगा। कभी बंद नहीं होना है। आज उत्पत्ति है तो कल प्रलय, आज सृजन है तो कल संहार। यह तो उत्पत्ति, प्रलय, संहार अनादि काल से चला आ रहा है, इसमें कभी कमी होनी नहीं है। उत्पत्ति करके पूर्ण, पालन करके पूर्ण, संहार करके पूर्ण। क्या कमी है?
यह प्रतीत होते हुए भी न बना है और न किसी ने बनाया है। यह प्रपंच भास क्यों रहा है? तो भैया ! यह कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज होती है, वही भासती है। जो नहीं है वह भी दिखायी देती है। आकाश में नीलिमा दिख रही है, वह नहीं है फिर भी दिख रही है। रज्जु में सर्प नहीं है फिर क्यों दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। मृग-तृष्णा में जल नहीं है, फिर क्यों नदी दिख रही है? दूँठ में पिशाच नहीं है, फिर क्यों दिख रहा है?
एक अंधा और एक आँख वाला रास्ते में दोनों आँधी में पड़ गये हैं, तो इस आँधी में बेचारा अंधा, उसकी तो आँख ही नहीं है, किसी न किसी खड्डे में गिर जाता है और आँख वाला मनुष्य कोर्ड न कोई सहारा, आधार को पकड़ लेता है और वह नहीं उड़ता, बच जाता है। इसी तरह संसार में दो तरह के मनुष्य होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी आँख वाला है और अज्ञानी अंधा और दोनों के लिए माया रूपी आँधी आती है। जब माया रूपी बवंडर आ जाता है तो दोनों उसमें पड़ जाते हैं। जानी फटाफट अपने ज्ञान से आत्मा रूपी खम्भा में आत्मा ब्रह्म परिपूर्ण है। मुझ आत्मा में क्या होने-जाने वाला विचारहीन अज्ञानी, बुद्धिहीन, अंधा विषय रूपी गड्ढे में कहीं न कहीं गिर जाता है।
एक बार एक नदी में पानी बढ़ा हुआ था। कुछ पथिक नाव से नदी पार कर रहे थे। उस नाव में एक मस्त भी बैठा था। जब नाव बीच दरिया में आयी तो बड़ी जोर से तूफान आया-मल्लाह को जब तूफान आता दिखाई दिया तो वह घबरा गया। उस समय वह मस्त कहता है-अरे मल्लाह तू क्यों घबरा रहा है। तब मल्लाह कहता है- 'हुजूर! तूफान आ गया है। अब बहुत करीब है और नदी का किनारा दूर है, अब मैं कुछ नहीं जानता, क्या होना?" तो मस्त हँसता है और कहता है-
काँपता है दिल तेरा अंदेश-ए-तूफाँ से क्यों ॥
क्यों घबरा रहा है. जबकि -
नाखुदा तू बहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू ॥
यह दरिया भी तू है और साहिल (किनारा) भी तू है। जब तेरा ही खेल है, तो मरा क्यों जाता है। ज्ञान तक तो त्रिपुटी रहती है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यहाँ तक ज्ञान है और जो गुणातीत पद, अमनस्क पद, स्वभाव पद, सहज पद, तूष्णी पद पर स्थित है, जहाँ न सत् है, न रज, न तम, न जीव भाव, न मुक्त भाव, न आत्म भाव, न ब्रह्म भाव, न मोक्ष भाव, न बद्ध भावा इन सब भावों के अभाव का नाम गुणातीत पद है।
यह संसार बिजली का ए.सी. करेन्ट है। बिजली के दो प्रकार के करेन्ट होते हैं-एक ए.सी. और डी. सी.। डी.सी. करेंट इतनी खतरनाक नहीं होती। इसके छू जाने से मरोगे नहीं यह दूर फेंक देती है। परन्तु, ए.सी. करेन्ट बड़ी खतरनाक होती है। जरा-सा स्पर्श किया नहीं कि बस चिपक गये। ऐसे ही यह सब संसार ए.सी. करेंट हैं। जरा-सा लगाव हुआ नहीं कि बस चिपक गये। जैसे-बहुत से साधुओं के पास कुटी नहीं रहती तो वे समझते हैं कि चलो बरसात में सिर ढाँकने के लिए जगह हो जाय तो अच्छा रहता, इस एक कुटिया बन जाती है। बाबा जी एक झोंपड़ी बना लेते हैं बस ए.सी. करेंट लग गया। अब कुटिया बन गयी। भगत लोग गुरु-पूर्णिमा में आयेंगे तो उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। दालान बना। दुनिया में हम यही देखते हैं। जरा यह संसार का लगाव लगने की देरी है, फिर कोठार-भण्डार भी बना। बस, गीता फैलने लगी। फैलते-फैलते चूल्हा भी आए, चक्की भी लगी, तो फिर उसकी अधिकारिणी भी आनी चाहिए। फैल गयी गीता। इतना कह देना काफी है। अक्लमन्दे इशारा काफी अस्ता जब बाबा लोगों का यही हाल है, तो गृहस्थियों को क्या कहें। तुम्हारे लिए तो जरूरी है। पहले दो प्राणी थे तब एक ही घर में काम चल जाता था। फिर बेटे हुए पुत्र-वधु आयी तो बेटे-बहु कहाँ रहेंगे? बस, ऐसा ही समझ लो। गीता फैल रही है। तुम्हारे पास और कोई गया वह भी चिपक गया।
समझो संसार से सावधान रहो। ए.सी. करेंट से दूर रहो। बोधवान होकर भजन करो। यदि, विद्वान हो तो जनता का कल्याण करो। भला करो। चाहे जिस सम्प्रदाय के हो।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ।
फिकर सभी को खा गई फिकर सभी का पीर ।
फिकर की फांकी जो करै ताको नाम फकीर ॥
संसार सिनेमा है, नकली है। इसे दूर से देखो। सत्य क्या है-परमात्मा । और असत्य है-संसार। संसार को देखना हो तो दूर से देखो और भगवान को देखना हो तो नजदीक से देखो और इतने नजदीक से देखो कि अपने से भिन्न मत देखो तब भगवान दिखेगा।
ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥
(गीता 15/1)
वेदों को संसार-वृक्ष का पत्ता क्यों बताया है? क्योंकि, जिस वृक्ष में पत्ते नहीं होते, वे सुन्दर नहीं लगते, सुशोभित नहीं होते। ठूंठ थोड़े ही अच्छा लगता है। ऋग, यजुर्व, साम, अथर्व वेदों में कर्मकाण्ड का विषय दर्शाया है। स्वर्ग-नरक और अनेक कर्मों का वर्णन हुआ है, ये सभी वेदों में आते हैं। है। स्वर्ग-न के आवागमन का चक्कर लगा रहता है। भगवान इन्हें पटो इसीलिए कहते हैं कि इनसे आवागमन का चक्र लहलहाता रहता है। संसार रूपी वृक्ष में कर्म जाल न होगा, तो ढूँठ ही हूँठ रह जायेगा। इसलिए लहलहाने दो-
अथश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥
(गीता 15/2 )
यहाँ तो भगवान ने ऐसा बताया है और श्रीमद् भागवत में जहाँ भगवान की गर्भस्तुति की गयी है, जन्म के समय -
एकायनोऽसो द्विफलस्त्रिर्मूलश्चतुरसः पंचविधः षडाटमा ।
सप्सत्वगष्टविटयो नवाक्षो दशच्छदीद्विखगो ह्या दिवृक्षः ॥
(27/दसम् स्कन्ध 10/2 / 27 )
श्री रामायण के उत्तरकाण्ड में वेदों ने श्री भगवान के राज्याभिषेक में स्तुति की है।
अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने ।
षटकंध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने ॥
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे ।
पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे ।।
(रा.उ. वेद स्तुति छं. 5)
यहाँ पर भी संसार वृक्ष का यही भाव है -
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेनं सुविरुद्मूलमसङ्गशस्त्रेण हढ़ेन छित्वा ।।
(गीता 15/3)
वाह भाई-इस संसार का कोई रूप नहीं है। न इसका आदि है, न इसका मध्य है और न अन्त है। न इस प्रपंच का, कहीं पर भी इब्तिदा है (शुरू है), न इन्तिहा है (आखिरी है) और न इसका दर्मियान है (मध्य है)।
असंग शस्त्रेण-इस वृक्ष को कैसे काटना चाहिए, कौन-सी कुल्हाड़ी से काटना चाहिए। ये एकादश है -
अमूलमेतद् बहुरूपरूपितं मनोवचः प्राणशरीरकर्म ।
ज्ञानासिनोपासनयति शिवेनच्छित्वा मुनिर्गों विचरत्यदृष्णः ॥
(श्रीमद् भा. 11/28 / 1 )
फिर इसे कैसे काटें? वैराग्य शस्त्रेण। वैराग्य शस्त्रस्य कि लक्षणम्।
देखो-
दृष्टिं ब्रह्म मयिं कृत्वा .... ।
किसी भी चीज को नारायण-आत्मा के अतिरिक्त उसका अस्तित्व न मानना, यही असंग शस्त्र है। यदि सत्य घनभूत 'मैं' से भिन्न किसी भी चीज को मानते हो तो संसार का जड़ मजबूत होता है और जब अपने से भिन्न न जानो तो यही संसार को काटने की युक्ति है। जहाँ पर तुम्हें स्थूल, सूक्ष्म संसार दिखाई पड़े वहीं हथियार से काट दो 'मैं हूँ।' बस, काट दिया। सिवाय 'मैं' आत्मा के कुछ है ही नहीं। एक तिनके को भी अपने स्वरूप से अलग न मानो।
यहाँ पर विषय अध्यारोप और अपवाद का है। यह संसार हुआ-हुआ सा भास रहा है, अनबना-बना सा भास रहा है। माता श्रुति से महात्माओं ने अज्ञानी बालकों को समझाने के लिए नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा समझाया है कि किसी प्रकार से यह दृश्य आँखों से ओझल हो जाये। नारायण के सिवाय कुछ दूसरा न भासे। इसलिए रामायण, भागवत् शास्त्र-पुराण आदि में संत-महात्माओं ने नाना प्रकार से दृष्टान्तों द्वारा समझाया है। यह भी अध्यारोप है।
सोकामयत बहुष्यां प्रजायेति स तपोतप्यत ।
स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किं च तत्सृष्ट्रवा तदेवानुप्राविशत् ॥
'मैं एक हूँ और अनन्त हो जाऊँ' - श्रुति इसलिए कहती है कि जिसकी स्थूल बुद्धि है जो, अजातवाद नहीं समझ सकते, उसकी समझ में आ जाये। भगवान ने ही यह संकल्प किया कि मैं एक हूँ और अनन्त हो जाऊँ, इसलिए भगवान सब कुछ नाम रूप में ही हैं। भगवान ही नाना रूप धारण कर, संसार बनकर इसी में प्रविष्ट हो जाते हैं।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥
(गीता 9/19)
'मैं' ही अमृत हूँ, 'मैं' ही मृत्यु हूँ। 'मैं' ही सत् हूँ, 'मैं' ही जड़ हूँ। 'मैं' ही चेतन हूँ, इसलिए कि संसार-पना इसकी आँखों से निकल जाय, इनकी आँखों में भगवान ही भगवान दिखे। सबको दण्ड प्रणाम करना चाहिए. क्योकि जीव रूप से भगवान सभी में प्रविष्ट हैं।
यदि संसार की उत्पत्ति मानते हो तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि जब संसार पैदा हुआ तो पैदा होने के पूर्व इसका क्या स्वरूप था। सत्य था कि असत्य था। भाव रूप था अथवा अभाव रूप था। यदि सत्य था तो फिर श्रीमान् जी सत्य की तो उत्पत्ति ही नहीं होती। सत्य मानकर संसार की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती और यदि संसार बनने के पहले अभाव रूप था तो अभाव तो असत्य होता है। इसलिए संसार को असत्य मानकर भी इसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। यदि, कहो कि संसार सत्यासत्य है तो भी नहीं बनता। इसलिए, संसार किसी भी हालत में पैदा हुआ ही नहीं। यह बंध्यापुत्रवत् है। यहाँ पर जिज्ञासु प्रश्न करता है कि संसार को बंध्यापुत्र कहा है। बंध्यापुत्र तो दिखता नहीं, परन्तु यह संसार तो दिख रहा है। भैया, बंध्यापुत्र से अनुत्पत्ति अंश लेते हैं। पैदा हुआ ही नहीं। यदि, कहो-किसी युवती का मुख 'चन्द्रमुख' है। चन्द्रमा के समान मुख है। चन्द्रमा थाली-सा दिखता है और उसका मुँह तो ऐसा नहीं है। चन्द्रमा से हम कान्ति भाग लेते हैं।
माया से इसकी उत्पत्ति भले ही मान ले। जैसे- इन्द्रजाल का इन्द्रजाली पैसे-पैसे के लिए इधर-उधर घूमता रहता है, वैसे वह हजारों की ढेरी लगा देता है। क्या ये रुपये-पैसे सत्य हैं। इन्द्रजाली सिर काट देता है और फिर काट कर जोड़ देता है। क्या सचमुच सिर कटा? क्या कटा हुआ सिर फिर जुड़ेगा। नहीं, सब असत्य है। इन्द्रजाली के इन्द्रजाल को देखकर बड़े- बड़े विमुग्ध हो जाते हैं। परन्तु, जो इन्द्रजाली का दोस्त होता है, जो उसका यार होता है वह उसकी पोल जानता है। यह संसार है इन्द्रजाल और इन्द्रजाली है स्वरूप आत्मा। उसी में इन्द्रजाल दिख रहा है। जिसने इन्द्रजाली भगवान आत्मा से याराना किया है वह इस इन्द्रजाल संसार से विमुग्ध नहीं होता। इसमें कभी नहीं पड़ता।
सो नर इन्द्रजाल नहि भूला । जा पर होइ सो नट अनुकूला ।
नटकृत विकट कपट खगराया। नट सेवकहि न व्यापइ माया ||
(रा. उत्तर)
इस पर एक आख्यान है श्रीमद्भागवत का। किसी समय जब भगवान लीलाधारी श्री कृष्ण वृन्दावन में लीला कर रहे थे, गोपियों ने भगवान से निवेदन किया कि भगवन् यमुना के उस पार महर्षि दुर्वासा पधारे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनका दर्शन कर आयें, भोजन करा आयों भगवान कहते हैं तुम्हारी जाने की इच्छा है तो जाओ, जब यमुना जी के पास पहुँची उस समय यमुना जी बढ़ी हुई थी और वहाँ यमुना जी को पार करने का नाव, (डोंगा) आदि कोई साधन न मिला। गोपियाँ निराश होकर वापिस भगवान के पास लौट आयी। भगवान ने पूछा कि यदि तुम लोगों का जाना जरूरी है तो हम एक मंत्र बता रहे हैं और इस मंत्र के प्रताप से यमुना मार्ग दे देंगी। गोपियों ने पूछा, क्या मंत्र है? भगवान ने मंत्र बता दिया -
यदि कृष्णो बालयतिः सर्वदोषविवर्जितः ।
तर्हि नो देहि मार्गं वै कालिन्दी सरिताम्बरे ।।
देखो तमाशा। यदि श्री कृष्ण जैसे कि वेद-शास्त्र, संत महात्मा बताते हैं कि अच्युतानन्द हैं, अखण्ड ब्रह्मचारी हैं, तो हे यमुने तू मार्ग दे दे। गोपियों ने इस मंत्र का पाठ किया तो यमुना में जल सिर्फ चार अंगुल रह गया। यमुना पार करके महर्षि जी के पास गयी। उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मन में तो पूजा की धुन थी। जब महर्षि जी को पूजन-भोजन करा चुकीं तो गोपियों ने आज्ञा मांगी वापस जाने के लिए। बाबा ने आज्ञा दे दी। गोपियों ने कहा कि जायें कैसे, यमुना तो बढ़ी हैं। बाबा पूछने लगे कि फिर आयीं कैसे। श्रीकृष्ण जी ने जो मंत्र दिया था वह गोपियों ने बताया और कहा इसी मंत्र के बल से यमुना ने मार्ग दे दिया। मंत्र को सुनकर बाबा हँस पड़े। बड़ा बढ़िया मंत्र है। हमारा भी मंत्र सीख लो यमुना से कहना कि बाबा दुर्वासा अगर कुछ भी न खाये हों, हाथ से भी न हुए हों तो माता यमुने मार्ग दे दे! यह मंत्र गोपियों ने कहा तो यमुना ने मार्ग दे दिया, क्योंकि बात सच्ची थी। इस पार गोपियाँ यमुना की रेती में सिर धरकर बैठ गयीं कि सरासर झूठों का बाजार गरमागरम है। श्रीकृष्ण भी झूठे, बाबा दुर्वासा भी झूठे और निगोड़ी यमुना भी झूठी जो गवाही दे रही है। यह रहस्य उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया। वृन्दावन में एक समय नारद जी आये। गोपियों ने यह प्रश्न रखा कि श्रीकृष्ण कैसे बालयतिः और दुर्वासा कैसे कुछ नहीं खाये। नारद जी ने बहुतेरा समझाया, परन्तु गोपियों की समझ में कुछ न आया? क्यों नहीं आया? इसलिए कि गोपियों को भगवान के वास्तविक स्वरूप आत्मा का बोध नहीं हुआ था। गोपियाँ भगवान के लीलाधारी स्वरूप की उपासिका थीं। लीला रूप में निष्ठा थी। एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान के साथ सब इकट्ठे हुए। उस समय भगवान ने अपने स्वरूप आत्मा का बोध कराया, तब यह रहस्य समझ में आया कि श्रीकृष्ण बालयतिः है और बाबा दुर्वासा भोजन नहीं किये। यह रहस्य ही ऐसा है, यद्यपि कुछ नहीं हो रहा है, संसार तीन काल में नहीं है। कौन मानेगा, जागने के बाद ही तो स्वप्न कहोगे। जब स्वप्न अवस्था में ही हो तब तो स्वप्न नहीं कहोगे। स्वप्न का द्रष्टा स्वप्नावस्था में 'मैं स्वप्न देख रहा हूँ ऐसा नहीं कहता। जब जागता है तब कहता है- 'मैंने स्वप्न देखा।' दुनियाँ रामायण पढ़ती है-
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सब सपना ॥
(रा.आ.)
इसलिए भैया संसार की उत्पत्ति तीन काल में नहीं है। सब कुछ नारायण ही है, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा जानो।
श्रुति भी तो जगत् की उत्पत्ति बताती है। भैया, जगत् की उत्पत्ति तो बताती है फिर अपवाद भी तो कर देती है। किस प्रकार -
अध्यारोपापवादाभ्यां निश्प्रपंचं प्रपंचते ।
जो परमात्मा ब्रह्म, सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मा को समाधि अवस्था में उन्हें वेद सुनाया, जिनकी कृपा से वेद प्रकट हुए, उनकी शरण में मैं हूँ। इससे मालूम होता है कि संसार पैदा हुआ है, लेकिन आगे चलकर श्रुति यह भी कहती है -
एकमेवाद्वितीयंब्रह्म नेहनानास्ति किंचन ||
एक ही चेतन परमात्मा है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। श्रुति के वाक्य में इतना विरोधाभास! तो कहते हैं, यहाँ विरोधाभास नहीं है। पूर्वा पर विरोध नहीं है। वह अध्यारोप है और यह अपवाद है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के एकसठवें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं -
एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबलाः।
अजीजनन्ननवमान्पितुः सर्वात्मसम्पदा ॥
श्री कृष्ण महाराज की सोलह हजार एक सौ आठ रानियों से एक-एक से दस-दस पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उसी के नीचे के चौथे श्लोक में श्री शुकदेव जी कहते हैं -
स्मायावलोक लवदर्शितभावहारि भूमण्डलप्रहितसौरत मन्त्रशौण्डे पत्न्यस्तु षोडशसहस्त्र मनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न शेकुः ॥
तो क्या पुत्र आसमान से आये? कहाँ से आये? सोलह हजार एक सौ आठ रानियों के मध्य में रहते हुए भी कामदेव भगवान श्रीकृष्ण में काम प्रदीप्त करने में समर्थ नहीं हुए। बिल्कुल उलट गया। यह क्या है? अध्यारोप और अपवाद। बिना बोध हुए यह चीज लगती नहीं है, समझ में शीघ्र नहीं आता। इसमें हर एक रानियों के दस-दस पुत्र हुए, यह अध्यारोप है और श्री कृष्ण भगवान आसकाम हैं, उन पर काम का कोई प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं हुआ, यह अपवाद है।
व्यालपास बस भये खरारी ॥
यह अध्यारोप है।
स्वबस अनन्त एक अधिकारी ।।
(रा.लं.)
और यह अपवाद है।
अभाव में भाव की उत्पत्ति का नाम अध्यारोप है तथा भाव और अभाव दोनों के अधिष्ठान को जानकर किये हुए अध्यारोप का खण्डन कर देने का नाम अपवाद है। इसका तात्पर्य लगाओ। श्रुति यहाँ ऐसी और वहाँ वैसी क्यों कही? देखो -
मृगतृष्णा की नदी बह रही है, उसे कोई छोटा बालक देखकर, अपने पिता से कहता है कि यह क्या बह रहा है? ये कैसी नदी है? कहाँ से निकली है? तीन काल में पानी नहीं है। एक बूंद भी नहीं, परन्तु बह रहा है। पिता ने सोचा कि अबोध बालक है। समझाने पर न समझेगा इसलिए कहा कि वटस, विंध्यागिरी पर्वत पर बंध्यापुत्र ने एक असत्य का तालाब खुदाया है। उसमें असत्य का जल भरा है। वहीं से यह नदी निकली है। अबोध बालक ने उसी को ठीक समझ लिया। जब बड़ा हुआ फिर मृगतृष्णा को देखा। फिर अपने पिता से प्रश्न किया कि यह क्या है? बुड्डे ने सोचा कि यह बालक नहीं रहा। बुद्धि में विचारशीलता पैदा हो गयी है। अब यह पहले जैसा कहने से न मानेगा। पिता ने कहा कि तुझे पहले बताया था कि विंध्यागिरी में बंध्यापुत्र के खुदवाए तालाब में असत्य का जल भरा है और नदी वहीं से निकली है। लड़का हँस पड़ा- वाह पिताजी, क्या बंध्या का पुत्र भी होता है। उसके पिताजी ने कहा कि नहीं, यह कुछ भी नहीं है। जूता उतार दो , लड़के ने जूता उतार दिया, पैर जलने लगे, छाले आ गये। पानी कहीं न मिला। फिर उसने सूर्य के तरफ दिखाकर कहा कि सूर्य भगवान का चमत्कार है। रेत में सूर्य की किरणों के पड़ने से ऐसा भास हो रहा है, पर है कुछ भी नहीं। अभाव में भाव बताकर सूर्य भगवान को अधिष्ठान बताकर असत्य जल का अभाव समझाया। नदी का प्रवाह है ही नहीं, बताया। अज्ञानी के लिए अध्यारोप और ज्ञानी के लिए अपवाद। संसार नहीं है ऐसा कहें तो इसे कौन मानेगा? वस्तुतः, था तो आत्मा, हूँ तो आत्मा और रहूँगा तो आत्मा। सिर्फ एक चेतन आत्मा परिपूर्ण अपनी महिमा में स्थित है।
आज का यह जो विषय है, इसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। गीता का पन्द्रहवाँ अध्याय -
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ||
(गीता 15/3 )
असंग का अर्थ होता है वैराग्या वैराग्य दो प्रकार का होता है। एक सोपाधिक और दूसरा निरुपाधिका घर में, समाज में या कहीं पर कोई हृदय में ऐसा विक्षेप पैदा हो जाय, जिसके कारण उसे विषयों से वैराग्य हो जाय। फिर वह विषयों से भागता है और किसी महात्मा से सटसंग द्वारा जब विवेक पैदा हो जाता है तब विषयों के अस्तित्व का त्याग हो जाता है। विवेक क्या है? नित्यानित्य विवेकः। नित्य वस्तु क्या है?
हूँ नहि तन मन वचन बुद्धि जाति वरण कुल एक ।
मैं हूँ चेतन सबन में याको कहत विवेक ॥
न तन, न मन, न वचन, कुछ नहीं, यह सब मैं नहीं हूँ, 'मैं' आत्मा हूँ। इस प्रकार का विवेक जब बुद्धि में आ जाता है तो विवेकनी बुद्धि द्वारा विषयों का जो विलास है इसको त्याग देना, इसको कहते हैं वैराग्य। यह निरुपाधिक वैराग्य है, जो विवेकनी बुद्धि द्वारा होता है। निरुपाधिक वैराग्य लाखों में एक को होता है। अधिक सोपाधिक वैराग्य होता है। यह एक जन्म के पुण्य के तप का फल नहीं है। वैराग्यवान को चाहिए कि जल्दी से जल्दी श्रुति, संत महात्मा की शरण में जाये। सिद्धः बोधवानः को विचरने की आज्ञा है, परन्तु वैराग्यवान को विचरने की आज्ञा नहीं दी जाती। इसलिए कि अभी इसको पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं है, गिर सकता है। अनेक जन्मों के पुण्य से इसे वैराग्य उदय हुआ है। ऐसा न हो कि संग-दोष से वैराग्य मन्द पड़ जाये। इसलिए उसे वैराग्य को एकान्त सेवन कर पकाना चाहिए- सुष्टन्याय के समान। खुष्ट कहते हैं-खूँटे को, जिसमें घोड़े आदि बाँधे जाते हैं। जैसे खूँटे को बार-बार ठोंक कर गाड़ा जाता है, मजबूती से, कहीं बलवान घोड़ा उखाड़कर भाग न जाय। इसी तरह वैराग्यवान को सात्विक आहार का सेवन कर, सत् ग्रंथों का अध्ययन कर, सत्संग द्वारा वैराग्य को पकाना चाहिए। वैराग्य को पकाया जाता है, क्योंकि यह डर है कि घूमेगा तो गिर जायेगा। प्रपंच में फँस जायेगा। कुटिया बनाने लग जायेगा, स्थान धारी हो जायेगा, रुपये कमाने में लग जायेगा और कीर्ति के साथ ब्याह कर लेगा। देखो भैया तीन बहने हैं-कीर्ति, कंचन और कामिनी। इनका वियोग एक क्षण के लिए भी नहीं होता। घर में सबसे बड़ी बहन पहले आती है-कीर्ति। फिर पीछे दोनों बहनों को आना ही है। कीर्ति, कंचन और कामिनी के साथ कौन ब्याह करता है? इसको लोकैषणा भी कहते हैं। ये ऐसी चुड़ैल है कि बड़े-बड़े साधुओं को हिमालय पर्वत की गुफा से कान पकड़कर मैदान में ले आती है और जैसे बन्दर साँप को पकड़कर पत्थर में रगड़ता है और कहता है 'फूँ'-'फूँ' इसी तरह से चुड़ैल मैदान में ले आती है और 'फूँ' 'फूँ' करके रगड़ती है, जिंदगी बरबाद हो जाती है। साधुओं से ब्याह करती है कीर्ति, हमारा नाम हो। अखबारों में नाम देते हैं और जहाँ कीर्ति बड़ी बहन आयी तो कंचन आनी ही है और फिर तीसरी बहन-गोविन्दाय नमोनमः । जिसने व्यक्तित्व की रक्षा की, वह कर्तव्य की उपेक्षा करेगा। व्यक्तित्व की रक्षा में कर्तव्य की उपेक्षा है। आज देख लो, नैतिक क्षेत्र में क्या, राजनैतिक, धार्मिक सभी प्रकार के क्षेत्रों में यही हालत है। कौन देखता है कि जनता कहाँ जा रही है। अपने व्यक्तित्व की रक्षा में सब मरे जा रहे हैं। कौन, किसको देखता है? क्या सुख है, क्या दुःख है। अपने आपको मिटा देना पड़ता है, तब कर्त्तव्य बनता है। कर्त्तव्य-परायण बनना कोई खाला जी का घर नहीं है। या तो व्यक्तित्व की रक्षा कर लो, या कर्तव्य की रक्षा कर लो। संसार में इस तरह रहना चाहिए कि कोई न जाने।
संसार-वृक्ष को कौन से वैराग्य से काटा जाय-सोपाधिक से या निरुपाधिक से। इस संसार वृक्ष को न सोपाधिक से काटो और न निरुपाधिक से काटो, बल्कि परम वैराग्य से काटो।
कहिय तात सो परम विरागी । दून सम सिद्धि तीनि गुण त्यागी ॥
(रा. आरण्य. 14/8) सूंघा,
जो कुछ सुनाई पड़े, भावना करो कि 'मैं' हूँ। जो कुछ नाक से भावना करो कि 'मैं' हूँ
दृष्टिं ब्रह्ममयीकृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत् ॥
देखो-सोपाधिक वैराग्य और निरुपाधिक वैराग्य तक तो विषय विलास का त्याग होता है, विषयों के अस्तित्व का त्याग नहीं होता। यह तो बोध होने पर ही होता है। इस वैराग्य में भोग से घृणा हो जाती है, परन्तु 'विषय' विषय रह जाता है और बोध होने पर यह 'विषय' विषय नहीं रहता, सब कुछ नारायण है। इसलिए उसके अस्तित्व का त्याग होता है। यही परम वैराग्य है, यही शस्त्र है। यह हथियार साथ में रखना चाहिए। भजन vec a . जप में, ध्यान में, धारणा में बैठे रहो। चाहे निरालम्ब ध्यान हो या सालम्ब, जिसकी जैसी साधना है, जहाँ तुमने 'मैं' हूँ भावना किया तो जानो उस वृक्ष को काट दिया। क्योंकि नाम रूप ही संसार है।
रघुपति भगति वारि छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे ।
तुलसीदास कह चिविलास जग बूझत-बूझत बूझे ॥
(विनय 124)
यहाँ तीन बार बूझत-बूझत बूझे कहा है। मन के शुद्ध हो जाने पर संसार चिविलास लगता है तो यह तीन बार बूझत-बूझत बूझे क्यों कहा? इसका क्या तात्पर्य है?
कोऊ कह सत्य झूठ कह कोऊ । जुगल-प्रबल कोउ माने ||
(विनय 111)
मानसकार कहते हैं कि तीनों भ्रम है। जहाँ पर त्रिपुटी है वहाँ तक सब भ्रम है। बूझत-बूझत और बूझे यही तीनों भ्रम है। यद्यपि, यह नारायण है, परन्तु जीव उसे संसार मानता है। अनादिकाल का 'यह संसार मानना' अभ्यास है।
अभी अनुभव कर लो। क्योंकि यहाँ तो सबको अनुभव कराया जा रहा है। जैसे, किसी चीज को देख रहे हो, दृश्य आता है, परन्तु दृश्याकार वृत्ति नहीं रहती। कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी कोई आया और तुम्हारे सामने खड़ा है, परन्तु तुम कुछ ऐसे तल्लीन हो कि उधर ध्यान नहीं दिया। तो तुम पूछते हो कि कब आये? सामने वाला कहता है कि घंटा हो गया, आपके पास बैठा हूँ। वेदान्त का स्वरूप बता रहे हैं, व्यवहार में। जिस समय कौन होठा है, कौन खड़ा है, इसकी तरफ वृत्ति नहीं जा रही है, उस समय सब कुछ 'मैं' हूँ। नाम, रूपाकार वृति बनी कि संसार खड़ा हो गया। 'मैं' हूँ बस फिर जैसी की तैसी स्थिति है। अभी जो ये बताये हैं न यह प्रक्रिया बड़ी विलक्षण है। दृश्य तो बाहर है ही नहीं। दुनियाँ इस प्रपंच से भागने की कोशिश करती है कि यहाँ बड़ा प्रपंच है। हिमालय की गुफा में रहो, परन्तु जाओगे कहाँ, वहाँ भी यह हल्ला तुम्हें सुनाई देगा। हल्ला हमारे हृदय में हो रहा है, बाहर नहीं है। जो देख रहे हो यह भीतर का दृश्य है। यह तुम्हारे स्वरूप से बाहर नहीं है। यह सब कुछ भीतर ही है। भीतर के विक्षेप का नाश हो गया तो बैण्ड बाजा भी बजता रहे चिंता नहीं है। अगर भीतर विक्षेप है तब पर्वत की कन्दरा में भी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें असली बात बता रहे हैं। परम वैराग्य का क्या स्वरूप है। यदि तुम राम के उपासक हो तो आप सहित सब कुछ राम है। यदि शिव के उपासक हो तो आप सहित सब शिव हैं। यही अभेद उपासना है।
यह अभेद कवच है। इस कवच को जिसने धारण किया, इसे धारण करने वाले के सामने एटम बम भी कुछ नहीं कर सकता।
![]()
![]()
![]()
टेप रिकॉर्डिंग द्वारा श्रुत प्रवचन का संक्षिप्त रूप (रायपुर 1963)
6. मन्मना भव मद्भक्तो
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमाटमानं मत्परायणः ।।
(गीता 9/34)
रास पंचाध्याई का पहला श्लोक -
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः ।
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥
(श्रीमद्भागवत् 10/29/1)
इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने पहले मन पैदा किया। लीलाधारी है, उन्हें मन की जरूरत पड़ती रहती है। कारण, मन के बिना लीला नहीं होती। भगवान का नाम है, चौराग्रगण्य। जिसके पास जो चीज नहीं रहती, उसी चीज को वह चोरी करता है। जिसके पास कपड़ा नहीं रहता, कपड़ा चुरा लेता है। जिसके पास धन नहीं रहता, धन चुरा ले जाता है। ऐसे ही भगवान के पास मन नहीं है तो मन चुरा लेते हैं। भगवान तो आप्तकाम हैं। परिपूर्ण हैं। कोई चीज की कमी नहीं है। परन्तु, भगवान के पास मन नहीं है। उसी की चोरी कर लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं, चित्त चोर हैं, जो कोई पास से निकला नहीं कि चित्त चुरा लेते हैं। सामना हुआ कि अन्टा-चित्त हो गया। मन हमेशा चुरा लेते हैं और अपने स्टाक में जमा रखते हैं। जब लीला करते हैं तब काम में लेते हैं।
जीव भाव तभी तक है, जब तक मन है। आत्म देश में मन नाम का पदार्थ नहीं है। 'मन्मना भव' कहने से भगवान का अर्थ यही है कि मन समर्पण कर दे। मन के समर्पण करने पर फिर कुछ देने को शेष नहीं रहता, वे दोनों एक हो जाते हैं। मन के देने के बाद जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। जब एकता हो जाती है, तभी भक्त की श्रेणी में आता है। तभी वह भगवान का सच्चा भक्त कहलाता है।
सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरणारि ।
भजहू राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि ॥
(रामायण उत्तर)
यहाँ विद्वत समाज है, पढ़े-लिखों का समाज है। जरा समझना, यहाँ खींचातानी का अर्थ नहीं है। पहले दोहे का अन्वय करो। हे उरगारि गरुड़, सैय्य भाव बिनु, सेवक भव न तरिया सेव्य कहते हैं, स्वामी को। तो सेव्य हुए भगवान परमात्मा और सेवक हुआ जीव। इसलिए सेवा करते-करते सेवक में जब तक सेव्य भाव नहीं आ जाता कि वह सच्चिदानन्द ब्रहा है तब-तक सेवक भव न तरिया क्या इस अर्थ में कोई शंका है? इस अर्थ का प्रमाण है -
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होइ जाई ।।
(रा. आयो.)
इसमें सेवक में सेव्य भाव आ गया है।
ब्रह्मवित् ब्रह्मव भवति ॥
(मुण्डक.उप. 3/2 / 9 )
इस प्रकार सिद्धांत विचार कर भगवान श्रीराम के चरण-कमलों को भजो, सेवन करो। किस भाव से? सेव्य भाव से। क्योंकि सेव्य भाव बिनु सेवक भव न तरिय और यह सेव्य भाव अभी आ जाय या जन्म जन्मान्तर के बाद आये, परन्तु जब तक सेव्य भाव से सेवक और सेव्य दोनों एक नहीं हो जाते, तब तक भव न तरिया प्रेम जगत् में भी यही बात है।
श्याम-श्याम रटते-रटते राधा श्याम भई ।
तब फिर पूछत यों सखियन से राधा कहाँ गई ।।
दोनों एक हो गये। कहने का सारांश यह है कि सारा दारोमदार मन पर है। इसलिए भगवान अर्जुन से कुछ न मांग करके, सिर्फ मन ही माँगते हैं। भगवान को देने योग्य, दातव्य वस्तु कोई है तो मन ही है। गुरु के लिए भी देने लायक चीज है तो अपना मन ही है। मन के ऊपर ही जोर क्यों दिया? क्योंकि जो चीज जिसकी होती है, उसी को वह दे सकता है। मन पर ही अपना अधिकार है और किसी पर नहीं। मन आत्मा की चीज है। अपना-आपका माना हुआ है। इसलिए मन पर अपना पूर्ण अधिकार है। तुम्हारी स्त्री पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारे पुत्र पर तुम्हारा अधिकार नहीं है।
ख्याल करो! यों तो तुम्हारा झूठा दावा है मन के ऊपर कि मन तुम्हारे अधिकार में नहीं है। जितने बैठे हो, हृदय पर हाथ रखकर बोलो, यह बात सत्य है कि तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है। झूठ न बोलना। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे अधिकार में न होगा, तब क्या कथा सुन सकते हो? जब सिनेमा के बैठे कौन सी समाधि करके जाते हो? बोलो, तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं में हो? अनुभव कर सकते हो? आफिस होगा सकते हो? तो फिर क्यों कहते हो कि मन बड़ा चंचल है, वश में नहीं क कर सामने कुछ कसर है? यह तो निर्विवाद सिद्धांत है कि हर एक का मन बाह हर एक के वश में हैं। बिना मन के वश में किये कोई काम हो ही नहीं सकता। नह आरओ, अब इस पर विचार किया जायेगा। अच्छा देखो, कोई ऐसा टाइम है भार जब कि यह अनुभव होता है कि मन चंचल है। वह कौन-सा टाइम है? पूजा मुल में, पाठ में, ध्यान-धारणा में बैठते हैं तब मन बड़ा चंचल हो जाता है, स्थिर भिन्न नहीं रहता। आप पूछते हैं, स्वामी जी एक बात है, जब पूजा-पाठ, ध्यान- है, धारणा में बैठते हैं तो यह मन विराद रूप क्यों धारण कर लेता है? और होल विषयों के अनुभव करने में मन को स्थिर करने के लिए कोई साधन करना अवर नहीं पड़ता, परन्तु पूजन में, पाठ में ही मन चंचल क्यों हो जाता है? यह है कि तुम्हारा प्रश्न है। अब उत्तर सुनो। विषयों के अनुभव काल में तुम्हारे अंदर मन' जीव भाव नहीं रहता, आत्म भाव रहता है। इसलिए मन का चंचलत्व प्रतीत स्वाभ नहीं होता है, क्योंकि आटम भाव में मन नाम की कोई चीज नहीं है। परन्तु नाम । पूजन में, पाठ में, तुम अपने को जीव मानते हो। जहाँ जीव भाव हुआ कि मनीराम वहाँ पहुँच जाते हैं। यह अमूल्य चीज है। फिर एक बार सुनो। प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक विषय के अनुभव करने में आत्म भाव रहता है और जिन आत्म भाव में मन का अत्यन्ताभाव है। मन उस समय, उस अवस्था में रहता ही नहीं इसलिए विषयों के अनुभव करने के लिए मन को स्थिर करने में आज ह कोई कठिनाई नहीं होती और पूजा पाठ, ध्यान-धारणा जीव भाव में करते कुछ ८ हो, इसलिए मन पैदा हो जाता है। मैं माला जपूँ, ध्यान- धारणा करूँ, यह बह जा भावना तो अपने को संसारी जीव मानते हो, तभी तुम्हें कुछ करने की इच्छा काल होती है। अपने-आपको तुमने संसारी जीव माना नहीं कि मन पैदा हो गया। बरह क्या भगवान की भी कहीं इच्छा होती है कि 'मैं माला जपूँ।' अभी जो कथा दौडोने सुन रहे हो यह जीव भी है वह सुरती है छ, है हनारायण भाव में सुन रहे है, यह हो। विषय समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या इस समय तुम्हें यह भाव होता वह आत होता है कि में सुन रहा हैं? किसी भी विषय के दर्शन काल में क्या भान होता ही जाये है कि में सुन रहा हूँ? किसी भी विषय के श्रवण-काल में क्या तुम्हें भान है कि मैं देख रहा हूँ, में सुन रहा हूँ आदि। इन क्रियाओं का अथवा इस प्रकार के कपिने का अनुभव तो जीव भाव में ही होता है। शब्द आदि विषयों का स्वाभाविक अनुभव, अनुभव काल में इसलिए नहीं होता कि अनुभव काल में आत्म भाव रहता है। श्रृंखला बंध गयी न। एक शब्द और बता दें। मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसका भी अनुभव नहीं होता। क्योकि आत्म भाव में अनुभव नहीं रहता। आत्म देश में अनुभव की चीज, अनुभवकर्ता और अनुभूति, तीनों नहीं रहते। यह त्रिपुटी नहीं रहती। स्वाभाविक विषयों के अनुभव काल में स्वाभाविक विषयों का अनुभव इसीलिए नहीं होता कि उस अवस्था में आत्म भाव रहता है। दर्शन काल में क्या द्रष्टा को दृश्य से अपनी भिन्नता का अनुभव होता है? नहीं होता। द्रष्टा दर्शन काल में दृश्य से अभिन्न होकर देखता है या मिन होकर? अभिन्न होकर? तब फिर द्रष्टा ही है, जिसका दूसरा नाम दृश्य है, दृश्य नहीं है। जब द्रष्टा दृश्य को देखता है, तब दृश्य से अभिन्न होकर ही तो देखता है, तब दर्शन कहाँ? केवल आत्मा ही आत्मा रह जाती है। इस अवस्था में त्रिपुटी नहीं रहती है, उस समय आत्म भाव रहता है। प्रश्न उठता है कि उस काल में मन रहता है कि नहीं? मन तीन काल में नहीं रहता। अगर मन रहता तो मन का स्वाभाविक स्वरूप चंचल है, उस समय मन का स्वाभाविक स्वरूप चंचलत्व प्रतीत होना चाहिए। इसलिए आत्मभाव में मन नाम का पदार्थ नहीं रहता। संकल्प-विकल्प ही मन का स्वरूप है।
जिसको फूलों से नफरत हो उसको खुशबू से वहशत हो ।
जिस दिल की मचलनी आदत हो फिर कोई उसे बहलाए क्यों ।॥
जिस नदी का स्वरूप ही बहना है तो क्या उसे कोई रोक सकता है? आज बांध दो लेकिन तुम्हारे बांध का कोई महत्व नहीं है। बांध बांधकर चाहे कुछ काल के लिए रोक लो। क्या वह रुकता है? किसी न किसी दिन वह बह जायेगा। यदि येन-केन प्रकारेण साधन करके रोक भी लो तो कुछ काल के लिए ही तुम ऐसा कर पाओगे। फिर क्या उसे रुका मानोगे? जिस वरह बलवान घोड़ा भाग रहा हो और तुम पकड़ने दौड़ो, जब पीछे पकड़ने दौड़ोगे तो वह घोड़ा जान जायेगा कि पीछे से उसे पकड़ने कोई दौड़ा आ रहा है, वह और दूर भागेगा। यदि तुम पीछा करोगे तो घोड़े को पकड़ न पाओगे। वह आगे दौड़ता ही जायेगा और यदि उसकी तरफ न दौड़ो। उसे भागने दो, तब वह ठहर जायेगा। भागेगा नहीं और थककर वापिस आ जायेगा, शांत हो जायेगा। यह एक युक्ति है। यह भी एक नीति है। लोग बीमारी फैलाते हैं, मन के पीछे परेशान होते हैं। मन को नहीं रोकना, यही मन के रोकने का साधन है।
धान रहा-पाठ, ध्यान-धारणा, जप इत्यादि में जब कोई बैठता है, उसी समय मन तंग करता है। मन की चंचलता भासती है। उस समय तुम अपने को क्या मान बैठते हो-जीव भाव या आत्म भाव? फिर ऐसी बीमारी क्यों फैलाते हो? यदि आत्मा मानकर बैठते तो इस आडम्बर की कोई जरूरत नहीं। फिर ये सब करने की तुमको आवश्यकता नहीं है। करना है तो बैठकर आत्म चिंतन करो। बाहर के आडम्बर की जरूरत नहीं, जब तुम अपने आपको आत्मा जानते हो। यदि मन की चंचलता स्वाभाविक न होकर बनावटी होती तो नष्ट हो जाती। पर, मन की चंचलता उसका स्वाभाविक स्वरूप है तो नाश कैसे होगा? नहीं होता। आँख का देखना स्वाभाविक है, कान का सुनना स्वाभाविक है। जब तक देखना है तब तक आँख है, जब देखना बंद हुआ तो आँख भी खत्म हुई। जब तक सुंनना है तब तक कान है, जब सुनना बन्द हुआ तो कान भी खत्म हुआ। यह स्वाभाविक है-अटल सिद्धांत है। मन है तो चंचलता है, चंचलता है तो मन है। मन नहीं तो चंचलता नहीं और चंचलता नहीं तो मन नहीं। प्यारे, तुम सच्चिदानंद आत्मा परिपूर्ण होते हुए भी अपने-आपको जब संसारी जीव मानने लगते हो तब टंट-घंट करने लगते हो, उस समय यह मन पैदा हो जाता है और तंग करने लगता है। इन सबसे बचना चाहो तो अपने-आपको जीव न मानकर, अपने-आपको परिपूर्ण सच्चिदानन्द आत्मा जानो। तभी इस मन पिशाच से बचोगे। अंधेरे में काले नाठा से बचना चाहो तो उस साँप को, रज्जु जानो। पिशाच से बचना चाहो तो ढूँठ जानो। ऐसे ही संसार से, माया से, प्रपंच से, मन से बचना चाहो तो अपने को व्यापक तत्व जानो। उस समय न मन है, न संसार है और न शरीर है। तीन ही चीज तो वेदान्त में समझना है। एक शरीर, दूसरा मन और तीसरी आत्मा। स्थूल पदार्थ में शरीर समझ लो। सूक्ष्म पदार्थ में मन और इन दोनों से परे शुद्ध सच्चिदानन्द आत्मा को जानो। बस, वेदान्त खत्म। दिन-दिन भर आफिस में काम करते हो। लाखों रुपयों का हिसाब करते हो, एक- एक पाई का हिसाब मिलाते हो। मजाल है मन टस से मस हो जाय और फिर पूजा-पाठ में, ध्यान-धारणा में ऐसे-ऐसे दृश्य आते हैं, जो लाखों बरस हुए मर चुके, आँखों के सामने खड़े हो जाते हैं। बताओ, अब उनकी क्या जरूरत है? उनके लिए यहाँ क्या पड़ी है? दुनियाँ तो देख रही है कि ध्यान में लगे हुए हैं, परन्तु वहाँ क्या मुसीबत बीत रही है। जिस मस्ती में मस्त होकर तुम्हारे व्यवहार हो रहे हैं, उसी मस्ती में यह भी भाव नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूँ, व्यापक हूँ, जीव हूँ, परिछिन्न हूँ। कुछ बनने में उपाधि है, न बनने में उपाधि नहीं है। सच्ची ईमानदारी और शराफत इसी में है कि कुछ मत बनो और यदि बनते हो तो दूसरे मुल्क पर हमला करते हो, कितनी आजादी है। कितनी बेखबरी है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो जंभाई भी आती है, मच्छर भी काटते हैं, नींद भी आती है, कमर में दर्द भी होता है। तब उठकर बैठ जाते हो। भाड़ में जाये ऐसा भजन, जमता ही नहीं। परन्तु, वैसा दिन भर सारा काम करते ही हो। बता सब कुछ दिए, नाच देखना है तो जीव मानो और मस्त रहना है तो मस्त हो ही। डण्ड, कसरत करना है तो करो, मिलना तो कुछ है ही नहीं।
अब इसको संत वाक्य करके और प्रमाणित कर दें। यह तो अनुभूतियाँ हैं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं -
मेरो मन हिरिजू हठ न तजें ।
निशि दिन नाथ देऊँ सिख बहु विधि, करत सुभाउ निजै ॥
रात-दिन इसको शिक्षा देता रहता हूँ, परन्तु यह मन मानता नहीं। फिर गोस्वामी जी दृष्टांत देते हैं-
ज्यों जुबती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुःख उपजै ।
हवै अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भजै ॥
संत महात्मा बड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं। कुछ छिपाकर नहीं रखते।
लोलुप भ्रम गृह पशु ज्यों जहँ तहँ सिर पदत्रान बजे ।
तदपि अधम विचरत तेहिं मारा कबहुँन मूढ़ लजै ॥
यहाँ मन के ऊपर दृष्टांत दिया है, युवती और कुत्ते का, अन्त में कहते हैं-
हौं हार्यो करि जतन विविध विधि अतिसै प्रबल अजै ॥
परन्तु इस मन को मैंने अजित पाया।
तुलसीदास बस होड तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजै ॥
(विनय पत्रिका 89)
मन बस में होता है, मगर कब ? जब मन का स्वामी-प्रेरक, प्रभु चाहे तो मन बस में हो जाता है। मन का स्वामी-प्रेरक कौन?
'उस देव को जानकर सर्व दुःखों से छुटकारा मिल जाता है' - ऐसा सुनकर जिज्ञासु शिष्य पूछता है 'को देवः ।' वह कौन देव है, जिसको जानने से सर्व दुःखों से छुटकारा मिल जाता है? जो तेरे मन को देखता है, जो तेरे मन का अनुभव करता है। "यो मनः साक्षी "वही देव है।
"यो मनः साक्षी" वह शिष्य और दो-चार महात्माओं के पास गया और यही प्रश्न किया। जब सभी से यही उत्तर मिला तब एकान्त में बैठकर सोचने लगा कि- "मनो मे दृश्यते मया" "अपने मन को देखने वाला तो मैं ही हूँ। दूसरा कोई नहीं।' वह फिर वापस महात्मा के पास गया और उसे फिर वहीं उत्तर मिला। 'जो मन को देखता है, मन का साक्षी है, मन का अनुभव करने वाला है, वही देव है।' 'मनोमे दृश्यते मया...।' मेरा मन ही मुझे दिखता है, तब मैं ही मन को जानने वाला हूँ। 'तर्हिदेवस्त्वमेवासि।' अरे, जिस देव को तू ढूँढ़ रहा है, वह देव तू ही है। दूसरा कोई नहीं। जैसे, तुलसीदास जी कहते हैं- 'प्रेरक प्रभु बरजै' मन का देव, मन का अनुभव करने वाला, मन को देखने वाला तो मैं ही हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मन मेरे वश में हो जाय, फिर क्यों नहीं होता? भैया, तुम चाहते तो हो, परन्तु तुम 'मैं मन का स्वामी हूँ' ऐसा समझकर कब चाहते हो, तुम किसी संत महात्मा के पास जाते हो तो कहते हो कि मन बड़ा चंचल है, कैसे वश में हो? मेरे प्यारे आत्मन्, मन को वश में करने के लिए साधन पूछ रहे हो और जब महात्मा पूछते हैं तो कहते हो कि मैं तो संसारी जीव हूँ। जब मन की महिमा इतनी लम्बी-चौड़ी गाते हो तो अपने को संसारी जीव मानते हो, तब मन तुम्हारे काबू में कैसे हो? चाहते तो हो मन अपने वश में हो जाय, परन्तु मन का प्रभु अपने को मानते नहीं, इसीलिए यह असाध्य बीमारी हो गयी है। क्या, ऐसा भी कोई टाइम है कि कभी मन बुरे में या भले में चला जाय और मैं न जानूँ? मन बुरे में जाता है तब मैं जानता हूँ, मन भले में जाता है तब मैं जानता हूँ।
मन नहीं है, इस अवस्था का दिग्दर्शन कराया गया। तुम्हें मन की चंचलता पसंद है तब अपने को जीव मानो और तुम्हें मन का अमन पसन्द है तो अमन पद में तुम सदैव विराजमान हो। अमन पद कोई बाजारु चीज नहीं जो मोल लेकर मिलेगा। अमन पद में निरन्तर बैठे हो। इसलिए -
मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥
(गीता 9/34)
'अरे ही स्वरूप-विस्मृति है' का भाव यह है कि आत्मा से भिन्न यदि कुछ भी भान होता है। तो यही अरे का स्वरूप है। जिस तरह अरे!!! भागो यह तो सर्प है, यह भय तो रज्जु में ही होता है न। बल्कि रज्जु ही है, जो अंधकार के कारण सर्प रूप में भासती है। इसी तरह अपना स्वरूप ही है, जो प्रपंच रूप में भास रहा है। वास्तव में माया, मन तथा संसार किसी काल में न तो था, न है और न होगा।
'निर्विकल्पता का विकल्प निर्विकल्पता का बाधक है।' इसका भाव यह है कि निर्विकल्प तो अपना स्वरूप ही है, जो कि बिना साधन के ही स्वतः सिद्ध है। अब साधन द्वारा निर्विकल्प होने की चेष्टा करना, यही निर्विकल्पता का बाधक है।
'आत्म चिंतन का संकल्प आत्म चिंतन में विक्षेप है।' इसका भाव यह है कि आत्मा से भिन्न कुछ भी न जानना, कुछ भी न देखना, कुछ भी भान न होना, यही आत्मचिंतन है। अब यदि आत्मचिंतन के लिए अलग संकल्प किया जाता है तो यही आत्मचिंतन में विक्षेप है। क्योंकि 'मैं' से यदि कुछ भिन्नता भासती है तो उसी समय आत्मचिंतन के लिए संकल्प होता है।
![]()
![]()
![]()
7.अव्यक्त-व्यक्त विवाद
(प्रेक्टिकल वेदान्त)
'तुझको अपने अवकाश पर इतना गर्व है कि अवकाश जिसकी देन है उसकी तरफ तू कभी नजर उठाकर भी नहीं देखता।'
'अरे यार अवकाश किसी की भी देन हो, परन्तु तुझ चैतन्यघन अव्यक्त को अवकाश-मंदिर में छिपाने की शक्ति रखता हूँ। यह मेरी ही महिमा है कि तू सर्व का सर्व होने के बावजूद आज भी तुझसे मिलने के लिए सारा संसार व्याकुल है। ब्रह्मादिक देवता भी चक्कर काट रहे हैं। मेरी ही बदौलत तो तेरा नाम पर्दानशीं हुआ। हालाँकि पर्दा फर्जी है। लेकिन कर्मों के कोप से, दुनियाँ फर्जी को सच मानती है। बस, यही अचम्भा है। शब्द से तेरे भाव की, अर्थ से तेरे रूप की, भाव से तेरे गुण की और लक्ष्य से तेरे कर्म की, निरंतर मैं तेरी रक्षा करता हूँ। इतने पर भी तू मुझको झिड़कियाँ देता है।' भूताकाश बोला।
'होश में आकर शब्द, अर्थ, भाव, लक्ष्य इन चारों की व्याख्या कर। मुझको क्या पता कि तेरी वजह से मेरा नाम पर्दानशी हुआ है। व्यक्तित्वहीन होने के कारण मैं गुप्त हूँ अथवा प्रगट हूँ इसका भी मुझको पता नहीं। ये सारे कलंक तेरे सिर पर, क्योंकि तू व्यक्तित्व रखता है। व्यक्तित्ववान के ही मुख पर कलंक-कालिमा दिखती है, व्यक्तित्वहीन पर नहीं। क्योंकि व्यक्तित्व ही प्रपंच का मूल कारण है। और व्यक्तित्व का ही नाम माया, जगत्, शरीर, इन्द्रियाँ, चतुष्टय अन्तःकरण, पंचप्राण, पंचकोष या सर्वदेश-काल-वस्तु, तीन गुण ये सभी व्यक्तित्व के अभाव में सर्व का अभाव है।' ऐसा चिदाकाश बोला।
'शब्द, अर्थ, भाव, लक्ष्य इन चारों का स्वरूप-भूताकाश शब्द है, प्रतीति अर्थ है, अवकाश भाव है, चिदाकाश! लक्ष्य है। ऐ पर्दानशीं चिदाकाश मेरा नाम भूताकाश तेरे भाव पर पर्दा है। भूताकाश नाम का अर्थ प्रतीति तेरे रूप पर पर्दा है। अवकाश रूपी भाव तेरे गुण पर पर्दा है और मुझ भूताकाश का लक्ष्य रूप चिदाकाश तेरे कर्म पर पर्दा है। ऐसा भूताकाश बोला।’
![]()
![]()
![]()
8. मैं 'मैं' का विवाद
यह कैसी आँख-मिचौली का खेल है कि सर्व का 'मैं' होते हुए 'मैं' की तलाश में दुनियाँ मारे-मारे फिर रही है। क्यों न फिरे। यदि वह 'मैं' होकर 'मैं' को ढूँढ़े तब तो वह प्राप्त करने में सरल और सुगम है। ढूँढ़ने वाला भी 'मैं'। ढूँढ़ता जिसे है वह भी 'मैं', परन्तु ढूँढ़ ने वाला अपने को कुछ का कुछ मानकर ढूँढ़ता है तो फिर 'मैं' कैसे मिलूँ। जब दोनों 'मैं', तो ढूँढ़ने का विकल्प क्यों? यार जब तू भी 'मैं' और 'मैं' भी 'मैं' तो क्या दो 'मैं' है? जी नहीं, 'मैं' ही 'मैं' हूँ। जब 'मैं' ही 'में'तो ढूँढ़ते किसको हो? 'मैं' को। यह विकल्प क्यों? यह विकल्प तब होता है जब 'मैं' में अमुक नाम की पूँछ लग जाती है। 'मैं' का ढूँढ़ना कब खतम होगा? इसकी आखिरी मंजिल कहाँ है? अमुक भाव का परित्याग कर देना ही 'मैं' की आखिरी मंजिल है। बस, ढूँढना खतम। मिल गया सनमा जल गया दैहरोहरम । जब तक मैं अपने-आपको अमुक मानता रहता हूँ तब तक ही ढूँढ़ने का विकल्प रहता है। अमुक भाव गया। 'मैं' मिल गया। पर बात एक और है। मैं, अपने आप 'मैं' को कुछ न मानूँ तो फिर तुझ 'मैं' को पूछेगा कौन? बोल सच बता, दिल पर हाथ रखकर ठीक- ठीक कह। अरे यार अमुक भाव तक ही तो मेरा महत्व है। अमुक भाव गया कि तेरा बड़प्पन गया। मटियामेट हो गया। ठीक है ऐ मैं ! ठीक है तेरा कहना। मगर मैंने तो तेरी परेशानी देखकर ऐसा कहा कि 'मैं' को पाना चाहता है तो अमुक भाव को छोड़। अरे ये जो 'मैं' कहता हूँ, यह क्या विवादग्रस्त है ऐसा कह वह 'मैं' चुप हो गया। अब जो शेष रह गया वह 'मैं' का 'मैं' ही रह गया। इसके सिवाय कुछ नहीं बचा।
![]()
![]()
![]()
9.विवर्त-विवर्तक
'विवर्त कैसा अनोखा जादूगर है कि असीम विवर्तक को अपने अभावांचल में छुपा रखा है।' इस मुक्त सूत्र की व्याख्या।
सबसे पहिली बात तो यह है कि विवर्त और विवर्तक किसको कहते हैं? विवर्त उसको कहते हैं कि जो तीन काल में न हो, परन्तु भ्रम के कारण सत्य-सा दिखाई पड़े और जिसमें दिखाई पड़े उसको विवर्तक कहते हैं। जिस प्रकार रज्जु विवर्तक है और सर्प विवर्त है। तो विवर्त रूप सर्प हुआ आनोखा जादूगर, क्योंकि जिस काल में सर्प भासता है, उस काल में रज्जु नहीं दिखाई पड़ती। यद्यपि, सर्प अभाव रूप है अर्थात् न तो प्रकाश में है और न अंधकार में ही, परन्तु विवर्तक रज्जु को अपने अभावांचल यानी नहीं रूप गोद में छुपा रखा है। इसी प्रकार रज्जु सर्प के दृष्टान्त से आत्मा और जगत् के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। 'मैं' आत्मा विवर्तक हूँ और सारा प्रपंच विवर्त है। वास्तव में यह नाम रूपात्मक सारा चराचर प्रपंच तीन काल में नहीं है, बंध्यापुत्र के समान है। खरगोश के सींग, आकाश में नीलिमा, मृगतृष्णा में जल, सीपी में में चांदी इत्यादि अभाव के समान यह संसार है, परन्तु 'मैं' आत्मा के न जानने पर अनादि काल से सत्य सा भास रहा है। बस, यही विवर्त का जादू है जो कि 'मैं' आत्मा आदि, मध्य, अन्त से रहित हूँ। फिर भी मुझ असीम आत्मा 'मैं' को अभाव स्वरूप जगत् प्रपंच ने अपने अंचल यानी गोद में छुपा रखा है। जिस प्रकार रज्जु ही है, जो कि सर्पाकार दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार 'मैं' ही हूँ, जो संसार के रूप में भास रहा हूँ। जिस तरह रज्जु के अनुभव हो जाने पर आकार-प्रकार वही रहता है, सिर्फ सर्प भाव नष्ट हो जाता है। इसी तरह अपने आपके दर्शन कर लेने पर प्रपंच का आकार- प्रकार सब कुछ ज्यों का त्यों ही रहता है, परन्तु जगत् दृष्टिकोण नष्ट हो जाता है। जैसा का तैसा 'मैं' ही 'मैं' रह जाता हूँ। जिस प्रकार रज्जु देश में सर्प नहीं है, सर्प देश में सर्प है। यदि, रज्जु देश में सर्प है तो प्रकाश में भी सर्प देखना चाहिए। सर्प तो अंतःकरण के अंदर रहता है, रज्जु में नहीं, बल्कि ज्जु को ही सर्प मानकर रज्जु से ही भय लगता है, क्योकि जिसको सर्प का ज्ञान नहीं है, उसको साक्षात् सर्प से कभी भी भय नहीं लगेगा, क्योंकि अर्थ से भय है, पदार्थ से नहीं। अर्थ विवर्त है, पदार्थ विवर्तक हैं। जैसे- किसी छोटे बालक को किसी भी हिंसात्मक जीव से भय क्यों नहीं लगता? इसलिए कि उस बालक के हृदय में अर्थहीन पदार्थ रहता है। शब्दादिक विषय भासते जरूर हैं, परन्तु किसी भी विषय का अर्थ बालक के भीतर होता ही नहीं। इसी कारण से भय तथा मान- अपमान इत्यादि का भान कभी नहीं होता। बालक मस्त रहता है। जो कुछ उपाधि है, अर्थ के ही लगाने में है। प्रदार्थ तो साक्षात् भगवान हैं। अर्थ को ही वेदान्त में अध्यास भी कहते हैं। अन्य में अन्य का भान होना, इसी का नाम अध्यास है। जिस प्रकार रज्जु में सर्प का भान होना, इसी का नाम सर्पध्यास है। इसी प्रकार अपने आत्म स्वरूप आत्मा (मैं) में जगत् का अनादिकाल से अज्ञान के कारण भान हो रहा है। किसी भी पदार्थ के अर्थ को माया भी कहते हैं और दूसरे शब्दों में इसी को जीव सृष्टि भी कहते हैं। जीव सृष्टि में ही जन्म-मरण, बंध-मोक्ष, पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म, नरक-स्वर्ग इत्यादि की कल्पना की जाती है। अब जिज्ञासु को विवर्त और विवर्तक पर फिर विचार करना चाहिए। जबकि, सारा प्रपंच ही 'मैं' आत्मा का विवर्त है तो यह बोध हो जाने पर विधि-निषेध जगत् का भी अभाव हो जाता है और सारी समस्याएँ हल हो जाती हैं। स्वरूप का ज्ञान होने पर जगत् का बाध होता है, नाश नहीं। बाध और नाश में अंतर है। जिस तरह आभूषण को गला देना, आभूषण का नाश है और आभूषण न मानकर सोना जानना, आभूषण का बाध है। इसी तरह इस भासमान जगत् को जगत् न मानकर अपना आप 'मैं' आत्मा जानना, यही जगत् का बाध है। जिस प्रकार रज्जु का विवर्त सर्प है, इसी प्रकार 'मैं' का विवर्त आकाश है। 'मैं' कितना असीम, अपार, अनन्त, अनिर्वाच्य, अमनस्क, अविचल, अखण्ड, अजर, अमर, अजन्मा और प्रत्यक्ष हूँ, परन्तु विवर्त स्वरूप अनोखे जादूगर आकाश ने अपने अभावांचल (गोद) में छिपा रखा है। जो जिसका आकार होता है वैसे ही आकार वाली वस्तु का उसमें भ्रम होता है। जिस प्रकार रज्जु का टेढ़ा आकार होता है इसीलिए टेढ़ा आकार वाला जो सर्प है, उसका रज्जु में ही भ्रम होता है। घट, पट आदि पदार्थ में सर्प का भ्रम कभी नहीं होता। तदाकारता में ही भ्रम होता है, अन्य आकार में नहीं। इसी तरह आत्मा आकाशवत् कही जाती है अर्थात् आकाश नहीं आकाश के समान जैसे- कहा जाय कि रज्जुनु सर्पवत् है अर्थात् रज्जु सर्प नहीं, बल्कि सर्प के समान है। इसलिए, भगवान आत्मा चराचर का 'मैं' आसमानी चादर से ढँका हुआ है। अतः, गुरु कृपा द्वारा आत्म विचार से आकाश रूपी चादर को उठा दो, फाड़ दो, आकाश, आकाश नहीं, बल्कि 'मैं' ही हूँ, ऐसी ज्ञानाग्नि से जला दो। 'मैं' चैतन्याकाश सागर में आकाश विवर्त को डुबा दो। महाकालेश्वर अल्मा भगवान शिव के तीसरे नेत्र ज्ञान रूपी प्रचण्ड प्रलयाग्नि से सनश्वर आत्मा भवन जादूगर अभाव रूप अनोखे ठग का सदा के लिए संहार कर दो। बस, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
10. आकाश समीक्षा
काश! आकाश आकाश होता, तब तो आकाश आकाश ही होता। काश! आकाश आकाश ही होता, तब आकाश को तिरोहित कौन करता?
आकाश तीखे स्वर में बोला- 'मैं आकाश महान न होता तो समस्त चराचर को अवकाश कौन देता।'
आकाश झाड़ी से मुस्कराकर बोला 'ऐ हमनाम ! तू काश चराचर का अवकाश है तो तुझ आकाश का कौन अवकाश है? काश! तू स्वतः सिद्ध है तब आकाश ही है। काश! तू परतः सिद्ध है तब तू है ही नहीं।'
आकाश दबे स्वर में बोला- काश! 'मैं आकाश न होता तो तुझ आकाश को छुपने का अवकाश कौन देता? मुझ आकाश के अवकाश मंदिर में ही तो तुझे आँख-मिचौली खेलने की जगह मिली है। 'मैं' कैसा अनोखा मंदिर हूँ! वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी कितने सुंदर चारों स्तम्भ हैं! पंच महाभूत कितना उच्च वैकल्पिक शिखर है! ऐसे अभाव रूप मंदिर में तू आकाश का आकाश, यानी मैं का मैं ही, जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों ही प्रसरित है। अमुक रूप कैसा बेमिसाल घूँघट है। ऐ परवानशीं, परदा उठा ! तेरे लिए दुनियाँ परेशान है, हैरान है, बेजान है। तू सबका सिरताज है, आफताब है, बेहिसाब है। तेरा दीदार हो जाने पर सारा आलम गफलत का ख्याले ख्वाब है। परदा फाश हो गया।
कहकहाकर बोला- 'अरे यार! परेशानी ही तो दुनियाँ की निशानी है और जो निशानी है वह लगबे फ़ानी है।'
बस, तमाशा खतम, रहा सनम का सनम, जल गया दहरो हरमा किधर गया मक्का, किधर गया बुतखाना? खुद की नजर से देखा तो मस्तों का मयखाना।
![]()
![]()
![]()
11. मन वश में होता है
अपने 'मैं' को कुछ भी न मानने पर ही मन वश में होता है।
यूँ तो मन के लिए अनादिकाल से नाना प्रकार के साधन, साधक गण करते चले आ रहे हैं और शास्त्रों में भी अनेक महर्षियों ने साधन बतलपाण करतेरमा मन को वश में करने का कोई भी समाधान किसी ने भी नहीं। है, लरखा है। मन के रोकने का साधन जरूर बतलाया गया है। वश में करना। तथा स्थिर हो जाना दोनों का मतलब एक ही होता है। जिस प्रकार नदी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है, न कि नदी को स्थिर करने के लिए। नदी तो समुद्र में ही पहुँचकर स्थिर होती है। बांध से नदी रुक तो जाती है, परन्तु बांध के टूट जाने का भय बना रहता है और वही नदी जब सागर में पहुँच जाती है तो अपने आप ही स्थिर हो जाती है। कोई भी जाकर समुद्र में नदी को हुए तो नदी का नामो-निशान भी कहीं नहीं मिलता। इसी प्रकार मन एक नदी है, कल्पना जिसकी धार है। अनेकों प्रकार के साधन मन रूपी नदी के रोकने के लिए बांध हैं। साधनों से मन रूपी नदी रुक तो जाती है, परन्तु वासना रूपी जल थोड़ा न थोड़ा निकलता ही रहता है और मन रूपी नदी जब आत्मानन्द सागर में पहुँच जाती है तब मन की हस्ती पूर्णतया मिट जाती है। क्योंकि, जिस प्रकार नदी का घर समुद्र है, उसी प्रकार मन का घर अपना स्वरूप आत्मा है। आकाश में पक्षी दिन भर उड़ता रहता है। जब तक अपने घोंसले में पक्षी नहीं आ जाता तब तक उड़ना बंद नहीं होता। इस प्रकार मन पक्षी है। संकल्प-विकल्प दोनों पंख हैं। विषयाकाश मण्डल में अनादिकाल से उड़ रहा है। जब तक अपने स्वरूप आत्मारूपी घोंसले में नहीं आ जाता, तब तक मन को शांति नहीं मिलती।
अब विषय यह है कि अपने 'मैं' को कुछ न मानने पर ही मन वश में होता है। उदाहरण, यह है कि संसार के हर एक काम में अथवा किसी भी विषय का अनुभव करने के लिए मन के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। अपने आप ही बिना किसी साधन के ही मन स्थिर अथवा वश में हो जाता है, क्योकि अनुभव करने वाला किसी भी विषय के अनुभव काल में अपने आप 'मैं' को कुछ भी नहीं मानता। अपने स्वभाव में स्थित रहता है और मन कहीं आता-जाता है तो मन के आने-जाने में किसी प्रकार का हर्ष-शोक भी नहीं होता, क्योंकि हर्ष-शोक जीव को होता है। स्वभाव रूप भगवान आत्मा 'मैं' को नहीं। इसलिए, स्वभाव में मन स्वाभाविक वश में होता है और परभाव अर्थात् जीवभाव में लाख कोशिश करने पर भी क्षण मात्र के लिए भी मन काबू में नहीं होता। जिसकी जो चीज होती है वहीं और उसी में वह स्थिर होती है। जिस प्रकार नदी समुद्र की है इसीलिए समुद्र में ही स्थिर होती है। नदी पहाड़ जंगल में नहीं। इसी प्रकार मन स्वभाव रूप आत्मा 'मैं'का है, जीव का नहीं। इसलिए मन को स्थिर अथवा वश में कोई करना चाहे तो अपने 'मैं' को कुछ भी न माने। केवल 'मैं' ही 'मैं' जानना चाहिए। यही परम शांति पद है। बस ! निजानन्द में मस्त रहो।
12. निर्जीव जगत् का अभिशाप
आज के भारतीय छात्र एवं छात्राओं की दशा देखकर कौन ऐसा अनुशासित हृदय नहीं होगा जो शोक के आवर्त में न पड़ जाय। दोष किसका है? अनुशासनहीनता का, पाश्चात्य सभ्यता का अथवा विकराल कलिकाल का। आइए, अनुशासनहीनता के संबंध में सबसे प्रथम विचार वाटिका का निरीक्षण करों प्राथमिक शाला से लेकर विश्वविद्यालय तक के छात्र-छात्राओं में अनुशासनहीनता का साम्राज्य व्यापक है। इसका कारण क्या है? गंभीरता से विचार करने पर पता चला कि वही छात्र-छात्राएँ अनुशासित होंगे, जिन पर उनके संरक्षकों का अनुशासन होगा। उदाहरण लीजिए-जैसे जिस मकान की नींव कमजोर होती है वह मकान चिरायु नह होता, जो बालक या बालिका अपने संरक्षक की आज्ञा का पालक होता है वहीं भविष्य में आगे चलकर प्रत्येक क्षेत्र का शिरोमणि बनता है। आज भौतिक जगत् के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कि नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अनुशासित न होने के कारण प्रायः निर्जीव अर्थात् चेतनाशून्य हो रहे हैं, दूसरे शब्दों में मरणासन्न हैं। अनुशासन एक ऐसा सुन्दर, पवित्र और भविष्य उज्ज्वल करने वाला शासन है कि इसके अभाव में सभी शासन केवल पाखण्ड मात्र हैं। अनुशासन की कक्षा माता-पिता के शासन से प्रारंभ होती है। माता-पिता का शासन प्राथमिक शाला है। आचार्य का अनुशासन माध्यमिक शाला है। शास्त्रानुशासन हाईस्कूल है और ईश्वरीय यानी सत्पुरुषों का अनुशासन विश्वविद्यालय है। प्राथमिक शाला का विद्यार्थी कमजोर है तो उसका विश्वविद्यालय तक पहुँचना असंभव है। घर के माता- पिता अथवा कोई भी संरक्षक वर्ग मोहासक्ति के कारण अपने बालक या बालिका पर अनुशासन नहीं रखते, यद्यपि रात-दिन देखते हैं कि मेरी संतान उच्छृंखल एवं अनैतिक कार्य में रत रही है, परन्तु यह सब देखने के बावजूद इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते कि कहीं भाग न जाय या आत्मघात न कर ले। परिणाम-स्वरूप संतान स्वच्छन्द और अनुशासनहीन हो जाती है। फिर भविष्य में सुधार होना संभव नहीं है। ऐसी संतान से क्या लाभ ? उसका जीवन काल स्वान-पुच्छ के सदृश है। जिस संतान से संरक्षक को समाज के सामने लज्जित होना पड़े, ऐसी संतान सर्वथा त्याज्य है। श्री मानसकार जी कहते हैं कि -
जाय जियत जग सो महि भारू । जननी जीवन विटप कुठारू ||
ऐसी संतान को देखकर लज्जा भी लज्जित होती है। अतः ग्राह्य नहीं है, भले ही हृदय को संताप हो। परन्तु, यह निर्विवाद सिद्धांत है कि इसके दोषी उसके संरक्षक वर्ग हैं। यहाँ पर दो बाते हैं-यह दोष या तो संरक्षकों में भी होगा, तब उसे देखकर संतान बिगड़ेगी अथवा संरक्षकों के द्वारा संतान अनुशासित नहीं होगी, तब बिगड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह रोग उत्तरोत्तर संक्रामक होता जा रहा है। भविष्य में माता-पिता को सिर पकड़कर रोने के अतिरिक्त और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि पाश्चात्य सभ्यता का प्रवेश द्वार अनुशासनहीनता है, क्योंकि अनुशासित हृदय में पाश्चात्य सभ्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। यूँ तो इस सभ्यता का साम्राज्य समस्त विश्व में व्यापक होरहा है, परन्तु भारत के तो रग-रग में और मुख्यतः छात्र एवं छात्राओं में पूर्ण अधिकार ही जमा लिया है। भविष्य में भारत से भले ही यह कोढ़ दूर हो जाय, परन्तु आधुनिक नवनिर्मित भारत का रोग शीघ्र निवृत्त हो जाना संभवनहीं। अब प्रश्न यह होता है कि अनुशासनहीनता, उदण्डता, उच्छृंखलता इत्यादि रोग के पैदा होने का कारण क्या होता है? समाधान-सहशिक्षा और सहशिक्षा का उपादान कारण है पाश्चात्य सभ्यता। विद्यार्थी जीवन एक महान पवित्र, तपस्वी, ब्रह्मचर्य जीवन है और यह जीवन ईश्वर जगत् का प्रवेश द्वार है। यह संयमी जीवन नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने का सुमेर है। मन, वचन, कर्म तीनों से भली-भाँति इसका पालन न होने से भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए, शिक्षा को अखण्ड ब्रह्मचर्य तप में आरूढ़ होना नितांत आवश्यक है। मान लो कि यदि विश्वविद्यालय की अंतिम डिग्री येन-केन प्रकारेण प्राप्त भी कर लिया तो इससे क्या लाभ ? कहीं से पैसा कमाकर पेट ही तो भर सकता है। इसका क्या महत्व है? पेट तो कूकर-सूकर भी किसी तरह से भर ही लेते हैं? यदि शिक्षार्थी जीवन में ही मानव-जीवन चरित्र का आदर्शमय निर्माण न कर लिया तो फिर भविष्य में क्या करेगा, क्योकि चरित्र के नाश में सर्व का नाश है और चरित्र के आदर्श में ही सर्व का आदर्श है। प्रकृति अथवा पुरुष, दूसरे शब्दों में छात्र हो या छात्रा, यदि चरित्रवान है तभी कुछ कर सकता है, कलंकित से क्या हो सकता है? नीति का, समाज का, धर्म का एवं युग का निर्माता और कोई दूसरा नहीं है, अपितु चरित्रवान ही है। इसका साक्षी डीतहास है। जबकि, ईश्वर को सिद्ध-असिद्ध करने वाले हम स्वयं है तो संसार का कौन-सा कार्य है कि जिसको हम न कर सकें। परन्तु हाँ, अनुशासित एवं चरित्रवान हों तब। ब्रह्मचर्य दो प्रकार का होता है, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। सतत् यानी निरन्तर अखण्ड आत्मा ब्रह्म का चिंतन करना अन्तरंग ब्रह्मचर्य है और मन, वचन, कर्म से निर्विकार होकर भली- भाँति वीर्य की रक्षा करना बहिरंग ब्रह्मचर्य है, परन्तु अंतरंग के बिना बहिरंग की रक्षा नहीं और बहिरंग के बिना अंतरंग की रक्षा नहीं। यदि, मन विकारवान होगा तो बिन्दुपात किसी न किसी रूप में अवश्य हो जायेगा, क्योंकि काम विकार का नाम है मनसिज अर्थात् जो मन से पैदा हो उसे मनसिज कहते हैं और आत्म चिंतन के बिना किसी का मन कभी भी निर्विकार हो जाय, आकाश में पुष्प के समान है। तात्पर्य यह है कि विषय चिंतन से मन निर्विषय नहीं होता, बल्कि निर्विषय जो आत्मा अपना आप है और जिसमें शब्दादिक विषयों की गुंजाइश ही नहीं, यानि जो शब्दातीत अथवा विषयातीत है, उसके ही चिंतन से मन निर्विकार होता है और निर्विकार क्या, मन की हस्ती ही मिट जाती है। मन की हस्ती मिट जाने पर सारे प्रपंच की हस्ती सदा के लिए परिसमाप्त हो जाती है। जब मन ही न रहा तो द्वैत कहाँ और जब द्वैत नहीं तब स्त्री-पुरुष का भेद कहाँ? सारांश, यह है कि संसार के अंदर कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, संन्यासी हो या तपस्वी हो, दिगम्बर अथवा वस्त्रधारी हो, बलवान अथवा निर्बल हो, बाल, युवा, वृद्ध हो, पढ़ अथवा अपढ़ हो, स्त्री, पुरुष, छात्र, छात्रा कोई भी हो जब तक अपने स्वरूप आत्मा 'मैं' को नहीं जाना, नहीं देखा, अनुभव नहीं कर लिया, तब तक आत्म चिंतन होगा ही नहीं और बिना आत्म चिंतन के मन निर्विकार नहीं होगा और बिना निर्विकारता के अन्तरंग ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं होगी। सारांश, यह है कि आत्मचिंतन मन से नहीं होता। जहाँ मन वाणी की गम नहीं उसका चिंतन मन से कैसे हो सकता है? जिस प्रकार प्रकाश से ही प्रकाश देखा जाता है, प्रकाश से ही प्रकाश जाना जाता है, प्रकाश से ही प्रकाश का चिंतन होता है, अंधकार से नहीं। इसी तरह आत्मा से आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा से ही आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा से ही आत्मा का अनुभव होता है, इसी प्रकार आत्मा से ही आत्मा का चिंतन होता है और आनने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला और चिंतन करने वाला भी आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। यह व्याख्या अन्तरंग ब्रह्मचर्य की हुई।
अब बहिरंग ब्रह्मचर्य वाटिका में विचरण करें। अन्तरंग तथा बहिरंग दोनों का एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, अन्योन्याश्रय भाव है, यानी एक- दूसरे के आश्रित हैं। जब तक बहिरंग ब्रहाचर्य पुष्ट न होगा तब तक अन्तरंग ब्रह्मचर्य (आत्म चिंतन) का पालन कैसे होगा। क्योंकि, विषय भोगी, विषय कीटाणु एवं विषयानन्द कलिल में सना हुआ व्यक्ति आत्म-चिंतन क्या कर सकता है। रात-दिन विषय विकारोत्पादक, देश, काल, वस्तु का सेवन करता हुआ मानव रूप में बिना सींग-पूँछ के महा पशु व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का नाम सुनते ही कालज्वर आ घेरता है। उसका इतना तप कहाँ कि ब्रह्मचर्य स्वरूप ब्रह्मलोक तक जा सके और थोड़ा बहुत जो कुछ रहा भी वह परिवार नियोजन प्रचण्डाठिन में भस्मसात् हो गया है। इसी पर श्री मानसकार का एक दोहा स्मरण आता है कि -
धरा न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे ।
जेहिं राखा रघुबीर, ते उबरे यह काल मंह ||
इसलिए छात्र तथा छात्राओं के नियम क्या हैं? ध्यान दीजिए। सबसे प्रथम सहशिक्षा से दूर रहना। पढ़ाई भले ही बंद कर दो, परन्तु वयस्क हो जाने पर एक कक्षा में एक साथ बैठकर अध्ययन करना शिक्षार्थी जीवन खतरे से खाली नहीं है।
उपन्यास तथा फिल्मी गीतों की किताबें पढ़ना या फिल्मी गीत गाना बन्द करो। सिनेमा जगत् के अंदर शिक्षणकाल में स्वप्न में भी प्रवेश मत करो। शिक्षार्थी को उचित है कि अपने संरक्षक अथवा आचार्य के अनुशासन में रहे। अभक्ष्य पदार्थ जैसे-मांस, मदिरा, अण्डा इत्यादि, अधिक मात्रा में कडुवा, तीखा, चरपरा, गरम मसाला, खट्टा तथा बासी इत्यादि पदार्थ का सेवन विद्यार्थी को कभी न करना चाहिए और जो भी देश, काल, वस्तु, छात्र एवं छात्रा के लिए विकारोत्पादक हों, वे सर्वथा त्याज्य हैं। उपरोक्त नियमों का पालन जो शिक्षार्थी करेगा वह समाज का आदर्श बनेगा, कुलभूषण होगा, राष्ट्र का कर्णधार होगा और भविष्य में ईश्वरीय विधान (सार्वभौम सिद्धान्त) का निर्भीक प्रचारक बनेगा।
नोट-वयस्क हो जाने पर जो भी छात्र और छात्राएँ शिक्षण काल में ही अपने देह, इन्द्रिय तथा मन पर पूर्ण अधिकार न पा सके तो उन्हें उचित है कि लज्जा, संकोच और भय का परित्याग कर अपने संरक्षक से कह देना चाहिए कि हमें शीघ्र गृहस्थ बना दीजिये। शिक्षार्थी यदि ऐसा न करेगा तो उसके पतन का भय अवश्यम्भावी है।
13. शिक्षा मानवता का स्रोत है
मानव वहीं है जिसमें मानवता हो, नहीं तो वास्तव में दानव है। मानवता यही है जो नीति के अनुकूल हो। नीति वही है, जिसका लोक परलोक में शस्माल हो। लोक वहीं है, जिसमें समस्त प्राणी वर्ग रहते हैं। परलोक वहीं है जहाँ पहुँचकर नर-नारायण हो जाता है, दूसरे शब्दों में जिसे संत जगत् कहते हैं। मानवता कोई बाजारू सौदा नहीं है। अनेक जन्मों के पूर्वार्जित पुण्योदय होने पर ही मानवता प्राप्त होती है। विद्या दो प्रकार की होती है। एक अपरा, दूसरी परा। अपरा विद्या मानव बनाती है और परा विद्या मानवता प्राप्त कराती है। शिशु कक्षा से लेकर संसार की जितनी भी विद्यायें हैं ये सभी अपरा हैं, अपरा विद्या के ही अंदर वेद-शास्त्र भी आ जाते हैं और परा विद्या उसे कहते हैं (जिसे अध्यात्म विद्या भी कहते हैं) जिसके द्वारा व्यापक तत्व जो सारे चराचर का 'मैं' है, जिसे जानकर नर से नारायण हो जाता है, जीव बंध-मोक्ष से मुक्त होकर आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। वास्तव में शिक्षा वही है, जिसको प्राप्त करके जीव अध्याटम जगत् में प्रवेश पा सके और यदि प्राइमरी से आदि विश्व-विद्यालय की भी मान्यता प्राप्त करके अनैतिक जगत् के गर्त की ओर जाता है, चरित्रवान, सदाचारी एवं समाज का आदर्श नहीं बनता, स्वयं का कल्याण तथा समाज और राष्ट्र के उत्थान करने में समर्थ नहीं होता तो वह जीवन मनुष्य जीवन नहीं है, वस्तुतः पशु जीवन है। ऐसे छात्र-छात्रा को लज्जा भी देखकर लज्जित होती है। उसका जीवन स्वान-पुच्छ के सदृश निरर्थक है। माता के युवावस्था रूपी वृक्ष को काटने के लिए मानो कुठार रूप है। आधुनिक जगत् में प्रकृति व पुरुष, दोनों समाज के अंतर्गत विद्वानों की कमी नहीं है, किन्तु आदर्श चरित्रवान प्रायः नहीं के समान हैं। यद्यपि, संसार में किसी भाषा का पठन- पाठन मानव जीवन को मानव बनाता है, बिगाड़ता नहीं। परन्तु, संग दोत्र के कारण वर्तमान काल की शिक्षा कलंकित हो रही है। अतः, संग दोष से बचने की नितांत आवश्यकता है, तभी शिक्षा मानवता का स्रोत है, अन्यथा व्यर्थ है।
14. समाज का आदर्श बनो
विद्यार्थी जीवन मानवता का स्रोत है। उन्नति और अवनति, सुसंग एवं कुसंग का परिणाम है। सदाचारता इस महान तपस्वी जीवन की रक्षा का परम साधन है। यह देव दुर्लभ मानव-जीवन ही अध्यात्म प्रदेश का प्रमुख द्वार है। गुरुजनों द्वारा अनुशासित रहकर जीवन को सफल बनाना प्रत्येक का कर्तव्य है। महान पुरुषों की कृपा का आकांक्षी होना निर्भयता का प्रतीक है। सत्पुरुषों की अनुकूलता विशुद्ध हृदय की परिचायक है। भगवान विश्वात्मा को बाहर भीतर से सर्वत्र देखना समस्त विकारों पर ऐतिहासिक विजय है। मन से सदैव सतर्क रहना मानवता का शस्त्र है। यह मन काग रूप है। हमेशा विषय रूपी विष्ठा पर ही चोंच मारता है। यह मन उलूक के समान है। इसे अज्ञान की अंधेरी रात ही प्यारी लगती है। ज्ञान के प्रकाश में तो मन की हस्ती ही मिट जाती है। यह मन स्वान के सदृश है। जिस प्रकार कुत्ता कहीं से सूखी हड्डी लाकर एकान्त में बैठकर बड़े चाव से चबाता है, हालाँकि चबाने से मसूड़ा छिल जाने के कारण स्वयं का ही रक्त हड्डी में लगता है और उसे बार-बार चाटता हुआ आनन्द मानता है, परन्तु मूर्ख स्वान यह नहीं जानता कि यह रक्त तो मुझसे ही निकला है। इसी प्रकार इस मन को विषयों द्वारा जो क्षणिक आनन्द प्राप्त होता है, उस विषय- जन्य सुख को विषयों से प्राप्त हुआ सुख मानता है। यह हरामखोर अज्ञानी मन ऐसा अनुभव नहीं करता कि आनन्द का भण्डार तो मेरे ही अंदर है अथवा आनन्द सागर तो 'मैं' स्वयं ही हूँ। अनादिकाल से नीति-अनीति का विचार न करके संसारी विषयों में भटक रहा है। इसलिए ऐसे धोखेबाज मन के लिए वीतराग सन्तों की कृपा ही अंकुश है। यह मानव-जीवन अनन्त जन्मों के भाग्य एवं भगवान के प्रसाद से मिला है, अतः अनैतिक कार्य पर दृष्टिपात मानवता पर कलंक तथा भगवान के विधान का उल्लंघन है।
15. सन्तों की अनोखी दृष्टि
भगवान को बिना जाने अनोखी दृष्टि नहीं आती।
शंका- भगवान को जानना क्या है?
समाधान - भगवान को मैंने जाना है, भगवान को मैं जानूंगा या भगवान को मैं जानता हूँ। ऐसा यदि कोई कहता है तो यह समझना कि उसने अभी तक भगवान को नहीं जाना। क्योंकि भगवान अपने आप से भिन्न कब था, जिसको मैंने जाना और भिन्न कब है, जिसे मैं जानूंगा अथवा दूसरा कौन जिसको मैं जानता हूँ। वास्तव में ये तीनों विकल्प हैं। न मैंने जाना है, न जाजूंगा, न जानता हूँ। यदि अपने आप 'मैं' आत्मा से भगवान भिन्न है तो वह भगवान नहीं और यदि अभिन्न है तो जाना है, जानूंगा या जानता हूँ, ये तीनों विकल्प नहीं। ये तीनों विकल्प 'इदं वाच्य' में होते हैं, 'अहं वाच्य' में नहीं। इदं वाच्य जगत् है, अहं वाच्य भगवान है। इदं वाच्य अमुक होता है, अहं वाच्य जिस पर अमुक का विकल्प होता है, वह अहं 'मैं' नाम से प्रसिद्ध भगवान होता है।
शंका- दिखना दिखता है या देखना दिखता है? यदि दिखता है तो देखे बिना दिखेगा ही क्या और देखना दिखता है तो दिखे बिना देखना कहाँ और जब तक किसी भी देश, काल, वस्तु, का विकल्प न हो तब तक दिखने-देखने का विकल्प कहाँ।
समाधान - सबसे प्रथम अमुक का विकल्प होता है, बाद में दिखने- देखने का, किन्तु देखने का जो विकल्प है उसमें ही दिखने देखने दोनों का विकल्प निहित है।
शंका- दिखने-देखने का जो विकल्प है, वह निर्विकल्प है या सविकल्प है? यदि निर्विकल्प है तो विकल्प, विकल्प नहीं और यदि सविकल्प है तो सविकल्प का कोई अस्तित्व नहीं।
समाधान- अरे भाई, विकल्प और विकल्पक का जो विकल्प है, यहभी तो विकल्प ही है और विकल्प-विकल्पक दोनों विकल्प जिस देश में,सूर्य में अंधकार के समान है, उसे भगवान कहते हैं और भगवान कहते ही जाना है, जानूंगा या जानता हूँ, देखा है, देखूंगा, देखता हूँ अथवा दिखना- देखना इत्यादि ऐसे उड़ जाते हैं, जिनका नामो निशान नहीं। जो शेष है वह अपना आप 'मैं' हूँ।
शंका- आत्म चिंतन का क्या लक्षण है?
समाधान- जिस चिंतन में चिंतन-अचिंतन दोनों विकल्पों का अभाव हो, चिंतन-अचिंतन दोनों में जो चिंतन हो, चिंतन का जो चिंतन, अचिंतन का जो अचिंतन अथवा चिंतन-अचिंतन दोनों भावों के अभाव का जो भाव, वही आत्म चिंतन है। आत्म चिंतन में देश, काल, वस्तु की अपेक्षा नहीं है। बिना चिंतन के ही जो सर्वकाल में स्वाभाविक चिंतन हो रहा है, वही आत्म चिंतन है। ऐसा आत्म चिंतन सारे चराचर का स्वतः सिद्ध है? यह आत्म चिंतन है, यह अनात्म चिंतन है-जब तक इस प्रकार का विकल्प रूप चिंतन है, तब तक आत्म चिंतन नहीं है, बल्कि विकल्प का ही चिंतन है।
गर्क हो जा रुहानी दरिया में, डुबा दे जिस्मानी खुदी को ।
फाड़ आसमानी चादर, बैठ जा लामहदूवी तख्त पर ॥
सन्तों की दृष्टि है, आत्मा की सृष्टि है, उपनिषदों की वृष्टि है, असली मुक्ता पिष्टी है ।।
'शिव' !!
।। श्री अच्युताष्टकम् ।।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ||1||
अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिका राधितम् ।
इन्दिरा मन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं संदधे ||2||
विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जानये ।
वल्लवीवल्लभा यार्चितायात्मने कं सविध्वंसिने वंशिने ते नमः ||३||
कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिथे ।
अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ||4||
राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यता कारणः ।
लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितोऽगस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम् ||5||
धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृ दूद्वेषिहा के शिहा कंस हृद्वंशिकावादकः ।
पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बाल गोपालकः पातु मां सर्वदा ||6||
विद्युदुबो तवत्प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत्प्रोल्लसद्भिद्यहम् ।।
वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहितांधिद्वयं वारिजाक्षं भजे ||7||
कुंचितैः कुन्तलेजिमानाननं रत्नमौलिंलसत्कुण्डलं गण्डयोः ।
हारके यूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणी मंजुलं श्यामलं तं भजे |8||
अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टवं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम् ।
वृत्ततः सुन्दरं कर्तृ विश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् ॥9॥
16. सन्तों की अनोखी दुनियाँ
दुनियाँ दुनियाँ ढूँढ़ती है, भगवान संत ढूँढ़ते हैं।
दुनियाँ दुनियाँ के पीछे चलती है, भगवान सन्त के पीछे चलते हैं।
दुनियाँ के लिए दुनियाँ प्रमाण है, भगवान के लिए सन्त प्रमाण हैं।
दुनियाँ के लिए दुनियाँ वैभव है, सन्त के लिए भगवान ही वैभव हैं।
दुनियाँ सम्मान का स्वागत करती है, सन्त अपमान का स्वागत करते हैं।
दुनियाँ किसी से राग और किसी से द्वेष करती है, सन्त राग से न राग, द्वेष से न द्वेष करते हैं।
दुनियाँ मृत्यु से डरती है, सन्त मृत्यु का आलिंगन करते हैं।
दुनियाँ अपने व्यक्तित्व की रक्षा करती है, सन्त अपना व्यक्तित्व खोकर सिद्धान्त की रक्षा करते हैं।
दुनियाँ अपवाद का प्रचार करती है, सन्त सिद्धान्त का प्रचार करते हैं। जो सार्वभौम अर्थात् निर्विरोध हो, उसे सिद्धान्त कहते हैं।
दुनियाँ आत्म विश्वास खोकर आपत्ति का नाश करती है, सन्त आत्म विश्वास की रक्षा के लिए आपत्ति का आदर करते हैं।
दुनियाँ युग का निर्माता किसी और को मानती है, सन्त नवयुग का निर्माण स्वयं ही करते हैं।
दुनियाँ जीव से ब्रह्म बनती है, सन्त ब्रह्म को भी भ्रम ही समझते हैं। दुनियाँ दिखने वाले को कुछ मानकर देखती है, सन्त दिखने वाले को देखने वाला ही जानकर देखते हैं।
दुनियाँ अज्ञान का नाश करती है, सन्त ज्ञान, अज्ञान दोनों का नाश करते हैं।
दुनियाँ बंध से मुक्त होती है, सन्त बंध, मोक्ष दोनों से मुक्त होते हैं।
दुनियाँ मन को रोकती है, सन्त मन के रोकने को रोकते हैं। दुनियाँ सिद्धियों को सिद्ध करती है, सन्त सिद्ध को सिद्ध करते हैं।
दुनियाँ समाधि में समाधिस्थ होती है, सन्त समाधि की समाधि अर्थात् परम-समाधि में समाधिस्थ होते हैं।
दुनियाँ दुनियाँ देती है, सन्त भगवान देते हैं।
दुनियाँ धनवान बनती है, सन्त दिवालिये बनते हैं।
दुनियाँ प्रपंच से संन्यास लेती है, सन्त संन्यास से संन्यास लेते हैं।
दुनियाँ भगवान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मांगती है, सन्त भगवान से भगवान को भी नहीं मांगते।
कुछ भी मत बनो, भगवान भी मत बनो, जैसे हो वैसे ही रहो, बनना ही है तो सन्त बनो।
17. सन्तों की अनोखी अनुभूति
जो माना जाता है, वह जगत् है और जो जाना जाता है, वह 'मैं' हूँ। अथवा जो माना जाता है, वह विवर्त है और जो जाना जाता है, वह विवर्तक है।
शंका-सबसे प्रथम किसने माना, किसमें माना और किसको माना?
समाधान- 'मैं' आत्मा अपने आपको मन माना। किसमें माना? 'मैं' में किसको माना? 'मैं' को ही। क्योंकि, जो सबसे प्रथम था, अब है, आगे भी रहेगा, वहीं से यह खेल शुरू हुआ। जो खेल के पहले था, वही इस खेल का खिलाड़ी है और खेल का जो देखने वाला है, वह 'मैं' ही हूँ। 'मैं'ने माना मन को। मन ने माना 'मैं'को। जो 'मैं' ने माना, उसका ही नाम मन अथवा माया है और मन ने जो माना, उसका ही नाम संसार है। मन (माया) का आधार 'मैं' हूँ और संसार का आधार मन है, जिसके अभाव में उसके माने हुए का अभाव हो जाय, वही संसार है। मानने वाले मन से संसार भिन्न नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में मन के अभाव हो जाने पर मन के माने हुए संसार का भी अभाव हो जाता है। किन्तु, मन के भाव-अभाव दोनों भाव में 'मैं' आत्मा ज्यों का त्यों ही रहता हूँ। इसलिए 'मैं' में ही सारा खेल है। यह खेल कब तक, जब तक खिलाड़ी 'मैं' आत्मा को नहीं जाना।
आश्चर्य तो यह है कि इन्द्रजाली के इन्द्रजाल का जिस प्रकार फोटो नहीं उतारा जा सकता, उसी प्रकार मन के माने हुए का भी चित्र नहीं उतर सकता। क्योंकि, यह अटल सिद्धान्त है कि मानने वाले का माना हुआ मानने वाले के ही अंदर होता है और मानने वाले से अभिन्न होता है। विश्व में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं जो अमुक का फोटो ले सके। अमुक मन रचित है, मन आत्म रचित है। इसलिए न 'मैं' का चित्र, न 'मैं' रचित मन का चित्र। जब मन का ही चित्र नहीं, तब मन के माने हुए प्रपंच का ही चित्र कहाँ? संसार मन के अंदर है। मन 'मैं' आत्मा के अंदर है। यदि 'मैं' आत्मा का चित्र होता तब तो मन का भी चित्र होता और जब मन का चित्र होता तो मन के माने हुए विकल्प रूप इन्द्रजाल जगत् का भी चित्र जरूर होता। 'मैं'तो समस्त प्रपंच का चित्र खींचता है। 'मैं' आत्मा का चित्र कौन ले सकता है? 'मैं सर्व का अनुभव करता हूँ। यही समस्त प्रपंच का चित्र खींचना है।
शंका- मन पदार्थ में जाता है कि विकल्प में जाता है? यदि पदार्थ में आता है तब तो वह पदार्थ 'मैं' ही हूँ, और यदि विकल्प में जाता है तो विकल्प का कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योकि श्रवण तो हो, किन्तु वस्तु का अभाव हो, उसे विकल्प कहते हैं।
समाधान- अरे भाई, मन न कहीं आता है और न कहीं जाता है। 'मैं' आत्मा कल्पतरु हूँ। मेरी ही छत्रछाया में बैठकर मुझमें ही और मुझको ही, मन कुछ न कुछ मानता रहता है। सारांश यह है कि किसी भी विषय का विकल्प करना, यही मन का जाना समझो और विकल्प न करना, यही मन का आना समझो। भला, जल को छोड़कर तरंग कहीं जा सकती है। इसी प्रकार 'मैं' आत्मा को छोड़कर मन कहाँ जायगा। मुझ आत्मा से अलग होते ही मन ही खत्म हो जाता है। तब आना-जाना किसका ? सब इन्द्रजाल है। इन्द्रजाली को भली-भाँति जान लेने पर इन्द्रजाली के इन्द्रजाल में मन कभी मोहित नहीं होता। इसी प्रकार इन्द्रजाली अपने आप आत्मा को भली- भाँति जान लेने पर विकल्प रूप इन्द्रजाल के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ सकता। इसलिए, मन न कहीं आता है और न कहीं जाता है और न मन के आने-जाने की कोई जगह है। हाँ, यदि अपने आपको जीव मानते हो, तब मन के रोकने का प्रयास करो और यदि अपने आपको आत्मा जानते हो तब तो सरकारी सांड़ के समान निर्द्धन्द्ध, निर्भय, स्वतंत्र तथा मस्त रहो। जैसे हो वैसे ही रहो। न कुछ दिखता है, न कुछ देखना है। 'मैं' जैसा हूँ, वैसा ही हूँ। मैं जो हूँ, सोई हूँ। 'मैं' सर्वत्र हूँ- यह देशवाची शब्द है। था, हूँ, रहूँगा, यह कालवाची शब्द है। 'मैं' सर्व हूँ-यह वस्तुवाची शब्द है। देश, काल, वस्तु ये तीनों 'मैं' आत्मा शिव में बंध्या पुत्र के समान हैं। यह कैसा अनोखा खेल, यह कैसा विवर्त-विवर्तक का मेल, यह कैसा अज्ञानियों का जेल, यह कैसी बढ़िया मन की नकेल।
संतों की अनुभूति है, मुक्त की विभूति है, मानने की रीति है, ज्ञान से प्रतीति है।
'शिव' !!
18. अध्यात्म और विज्ञान
1. आत्म रहस्य को अध्यात्म कहते हैं और प्रकृति रहस्य का नाम विज्ञान है।
2. अध्यात्म का फल है आंतरिक सुख और विज्ञान का फल है बाह्य सुखा
3. भौतिक जगत् में विज्ञान का साम्राज्य होता है और अन्टार्जगत् में अध्यात्म का।
4. भौतिक विज्ञान के अनुभव का नाम टेक्नोलॉजी है और अध्यात्म के अनुभव का नाम समाधि है।
5. विज्ञान जगत् की आधारशिला बुद्धि है और अध्यात्म जगत् की जिज्ञासा।
6. बाह्य सुख अचिर है और आंतरिक सुख नित्य अथवा चिर।
7. वैज्ञानिक जगत् की यात्रा का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि प्रकृति में नानात्व भाव है और अध्यात्म जगत् के प्रवास की चरम सीमा आत्मानुभूति है।
8. अध्यात्म प्रत्येक क्षेत्र में मानव-जीवन का उत्थान करता है और विज्ञान वैज्ञानिक को प्रकृति के अद्भुत रहस्य को जानने के लिए खोज की ओर अग्रसर करता है।
9. बाह्य जगत् तृष्णा का स्रोत है और अन्तर्जगत् तृष्णा का काल है।
10. अन्तर्जगत् पोस्टकार्ड है और बाह्य जगत् लिफाफा है।
11. प्रकृति का रहस्य रूप विज्ञान, जिसका मूलाधार अध्यात्म (आत्मा) का चमत्कार है। अध्यात्म, विज्ञान का यही समन्वय है।
12. बुद्धि की बुद्धि, चैतन्य घनभूत, सर्व का अस्तित्व, 'मैं' संज्ञा से अभिव्यक्त आत्मा के बिना वैज्ञानिक जगत् में प्रवास के लिए बुद्धि को प्रेरणा कौन देगा। अध्यात्म, विज्ञान का यही समन्वय है।
13. बाह्य जगत् में पर्यटिका बुद्धि को विज्ञान कहते हैं और अन्तर्जगत में पर्यटिका बुद्धि को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म, विज्ञान का यही समन्वय है।
19. विश्व धर्म
आज संसार में धर्मों की भरमार है। बड़े-बड़े विद्वानों ने समस्त विश्व के धर्मों की गणना दो हजार नौ सौ निनानबे बतायी है और जो भी गणना में आते हैं, वे सभी एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं अथवा राग-द्वेषी है और सभी धर्मावलम्बी अपने-अपने धर्म को अनादि बतलाते हैं। आज भी दिन पर दिन धर्म बनते ही जा रहे हैं। संसार की सर्वसाधारण जनता भ्रम में पड़ जाती है कि हम कौन से धर्म को मानें और किस धर्म का त्याग करें। यही कारण है कि पढ़े-लिखे लोग खास करके पाश्चात्य विचारधारा के व्यक्ति, धर्म के नाम पर नाक सिकोड़ते और धर्म चर्चा के स्थल से उठकर चले जाते हैं। वे क्यों न नाक सिकोड़ें या क्यों न उठकर चले जाएँ, क्योंकि धर्म के ही नाम पर तो अखण्ड भारत के दो टुकड़े हो गये। धर्म के नाम पर लाखों का बलिदान हुआ और रक्त की नदियाँ बहीं। आज भी धर्मान्धता एवं विचार शून्यता के कारण वर्तमान युग के भविष्य का इतिहास उज्ज्वल नहीं, बल्कि अंधकारमय है। उस धर्म का दूर से ही अभिवादन है, जो धर्म आपस में लड़ना-झगड़ना अथवा एक-दूसरे से भिन्नता की शिक्षा देता हो। ऐसा धर्म मानव धर्म या विश्व धर्म कहलाने का अधिकारी नहीं है। बल्कि, ऐसे धर्म को पशु धर्म कह देने में कोई अत्युक्ति नहीं है। क्योंकि, पशुओं का हृदय भी तो भिन्नता-अभिन्नता, धर्माधर्म, ग्राह्य-त्याज्य का विचार करने में मूढ़ होता है। वर्तमान काल में जितने भी धार्मिक स्थल हैं हिन्दुओं के हों, मुसलमानों के हों, ईसाइयों, यहूदियों, जैनियों, अथवा बौद्धों आदि के, सभी जगह राग-द्वेष का साम्राज्य है। कारण यह है कि धर्म का क्या स्वरूप है? मानव जगत् की क्या धारणा है? मानव अथवा विश्व का समस्त प्राणी वर्ग क्या चाहता है? कहाँ से और कहाँ को यात्रा हो रही है? जितने भी यात्री है सबकी आखिरी मंजिल अलग-अलग है या एक ही है? ... ऐसे विचार जगत् में कोई लाना ही नहीं चाहता। नदियाँ यदि आपस में लड़ती हैं तो यह कहना पड़ेगा कि नदियों ने अपने आपका व्यक्तित्व नहीं जाना। संसार में हम सब की गंगा से लेकर और एक गंदी नाली तक, एक ही आखिरी मंजिल है, एक ही घर हैं। इन सब बातों पर विचार न करने को ही अज्ञान कहा जायेगा। नदियों के बहने का मार्ग भले ही भिन्न-भिन्न हो, परन्तु नदियों का विश्राम स्थल तो एक ही है। नदियों के नाम रूप भले ही भिङ्ग- भिन्न हों, किन्तु जल रूप से तो एक ही हैं। नदियाँ वस्तुतः यदि एक-दूसर सिम एक है तब तो नदियों की यात्रा भी पृथक-पृथक स्थानों के लिए होनी साहिए। परन्तु नदियों का कितना विशाल भवन है और भवन कितना बाहिर तिल है। भवन का द्वार कितना गौरवशाली है कि द्वार पर पहुँचते ही मह गंगा हो अथवा किसी के घर की गंदी नाली, सभी अपनी-अपनी हस्ती मिटाकर (मैं अमुक हूँ), इस अहंकार रूपी सिर को द्वार पर ही रखकर, भीतर भवन में प्रवेश कर पाती हैं।
आइए, विचार वाटिका में सबसे प्रथम धर्म के अर्थ पर विचार करें। धर्म का अर्थ होता है धारणा। किसी भी हृदय की धारणा को ही धर्म कहते हैं। जब तक यह हृदय के अंदर है तब तक उसका नाम धर्म है और वही जब क्रिया रूप में आ जाता है, तब उसी का नाम कर्म हो जाता है। अब विचार करना है कि समस्त विश्व की धारणा एक है अथवा अनेक। किसी स्थान पर दस- पाँच व्यक्ति बैठकर विनोद के लिए आपस में कहने-सुनने लगते हैं कि भाई संसार में पैदा हुए हैं इसलिए अपने को क्या करना चाहिए। यानी हम मनुष्य हैं तो मनुष्य को क्या करना चाहिए दूसरे शब्दों में मनुष्य का क्या कर्त्तव्य है? यदि उस गोष्ठी में कोई संन्यासी बैठा है तो वह कहेगा कि प्रपंच का त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। यदि कोई विषयी बैठा है तब वह अपना राग अलापेगा। यदि धर्म या ईश्वर से विरक्त पुरुष है तब वह अपने ही स्वर में बोलेगा और यह मौलिक प्रश्न है कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है? इसी प्रकार इसका उत्तर भी सार्वभौम ही होना चाहिए। पूर्वोक्त प्रश्न का समाधान यह है कि मानव अनादिकाल से जिस वस्तु को ढूँढ़ रहा है, उसे प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का कर्त्तव्य है। क्या ढूँढ़ रहा है? आनन्द। कोई भी मनुष्य अथवा प्राणी की प्रवृत्ति जब किसी कार्य में होती है तो आनन्द को ही लक्ष्य मानकर होती है। संसार का कोई भी देश, काल, वस्तु प्रिय नहीं है। यदि प्रिय है तो आनन्द जिस सुख को एक व्यक्ति बड़े से बड़े पाप कर्म में ढूँढ़ता है, उसी को दूसरा व्यक्ति प्रपंच को ठोकर मार पर्वत की कन्दरा का सेवन करता है। नीति-अनीति, पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म, राग-द्वेष, निन्दा-स्तुति अथवा यूँ कहो कि जिसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य में, गृहस्थी स्त्री-पुत्रादिक में, वानप्रस्थी वानप्रस्थ में, संन्यासी संन्यास में, वैरागी वैराग्य में, चोर चोरी में, मद्यपी मद्यपान में, दुराचारी-दुराचार में सवाचारी सदाचार में, आस्तिक ईश्वर में तथा नास्तिक अनीश्वर में, निंदक हिंदा में स्तुतिवाला स्तुति में, रागी राज में, द्वेषी देष में। तात्पर्य यह है कि किसी भी विषय में जब कभी मन जाता है तो आनन्द की ही आशा से जता है। क्योंकि, आनन्द ही प्राणी मात्र की खुराक है। इसके बिना एक क्षण भी कोई जीवित नहीं रह सकता। आनन्द के वियोग में मानव आत्मघात कर लेता है। आनन्द यात्रा का आरंभ अनादि है और जब टाक आखिरी मंजिल लक्ष्य स्थान पर नहीं पहुँच जाता, तब तक यात्रा समाप्त नहीं होती। समस्टा विश्व एक ही प्रवाह में प्रवाहित है और एक ही स्थान को जीव जगत् का प्रस्थान है। अब प्रश्न होता है कि आनन्द तो क्षण-प्रतिक्षण शब्दादिक विषयों में मिलता ही रहता है तो यात्रा समाप्त हो जानी चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं। जिस आनन्द को संसार का प्राणीमात्र चाहता है या जिसके लिए सब कुछ न्योछावर कर रहा है, वह आनन्द कुछ और ही है। क्या संसार का कोई भी प्राणी ऐसा चाहता है कि हम 23 घंटा 59 मिनट आनन्द भोगें और एक मिनट दुःख ही सही, बल्कि सबकी यही इच्छा होती है कि हमें तो ऐसा सुख मिले कि सर्व दुःख दूर हो जाए, हमेशा हम सुखी रहें। सारांश यह है कि हर एक प्राणी कौन-सा सुख चाहता है, क्षणिक अथवा नित्य? टाब मुक्त कंठ से यही उत्तर मिलेगा कि नित्य। इससे यह सिद्ध हुआ कि विश्व का समस्टा प्राणी वर्ग विषय जन्य सुख अथवा विषयानन्द की खोज में नहीं है, बल्कि मित्यानन्द, दूसरे शब्दों में आनन्द सागर की ओर बहाव है। जिस प्रकार से समस्त नदियों का प्रवाह जंगल पहाड़ की तरफ नहीं, सागर की तरष्ठ है। अब विचार यह करना है कि सारे विश्व की धारणा एक है नित्य सुख की प्राप्ति और धारणा का ही नाम धर्म है। तब विश्व का धर्म एक हुआ और यह धर्म अकृत्रिम, व्यापक, अद्वितीय, अखण्ड, अविचल, अनादि, सत्य, सनातन, भारतीय इसी को मानव धर्म भी कहते हैं। इस धर्म पर जब कभी आपत्ति आती है, तभी भगवान अजन्मा का जन्म हुआ करता है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
(गीता 4/7)
अब प्रश्न होता है कि वह कौन-सा धर्म है, जिस धर्म की रक्षा के निमित भगवान का अवतार होता है अथवा जिसके प्रसार के लिए भगवद् विभूतियाँ भूमण्डल पर अवतरित होती रहती हैं। ग्लानि का अर्थ नाश नहीं होता, बल्कि छुप जाना या दब जाना है। जिस प्रकार नेत्र और सूर्य के बीच में घनघोर बादल के आ जाने से सूर्य नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य का नाश हो गया। बस, इसी का नाम ग्लानि है। प्रचण्ड वायु के चलने से बादल जब हट जाते हैं, तब सूर्य तो सभी नेत्र वालों को प्रत्यक्ष ही है। इसी प्रकार श्रुति-स्मृति के विरुद्ध सिद्धान्त पाखण्ड बादल करके यह भगवद् धर्म जब कभी लोप-सा हो जाता है यानी छुप जाता है, उस समय पाखण्ड रूपी बादलों को हटाने अथवा छिन्न-भिन्न करने के लिए जन-जन के हृदय में इस व्यापक विश्व धर्म का प्रसार करने के लिए नारायण रूप महान पुरुष आते रहते हैं। भगवान के अवतार चार प्रकार के होते हैं-नित्य, नैमित्तिक, प्रादुर्भाव और आतुरा नित्य अवतार रूप संत महात्मागण है- नैमित्तिक अवतार रूप भगवान राम-कृष्णादिक हैं और आतुर स्वरूप भगवान गजेन्द्रोद्धारक हरि हैं, तीन कार्य करने के लिए नैमित्तिक अवतार होता है।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।।
(गीता 4/8)
भक्तों का कल्याण, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। स्थापना का अर्थ बनाना नहीं होता, बल्कि स्थापित करना होता है। जिस धर्म को स्थापित करना है वह धर्म पहले से है। हाँ, उस पर से आवरण हटा देना है। भगवान का नित्य अवतार है, जो संत रूप में होता है वह केवल एक ही कार्य करता है-जन कल्याण अथवा जीव मात्र के अन्तःस्थल में भगवान का विधान स्वरूप सत्य सनातन धर्म की स्थापना यानी प्रचार। भगवान के विधान का स्वरूप -
ईशावास्यमिदꣲ᳜ सर्वम् ।।
(ईशा.उ. 1)
अथवा
योगांपश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥
नारायणेवेदꣲ᳜सर्वं। आत्मैवेद्ꣲ᳜सर्वं । अहमेवेदꣲ᳜सर्वं ॥
भगवान का यही अटल विधान है। इसी विधान द्वारा विश्व के हृदय का परिवर्तन निःसंदेह है और हृदय का परिवर्तन युग का परिवर्तन कहा जाता है। युग बदलने के लिए इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। हृवय अथवा युग के परिवर्तन में सभी का परिवर्तन है। हृदय (देश), युग (काल), वस्तु (व्यक्ति), इन तीनों में जो व्यापक सच सदैव अक्षुण विराजमान है, देश, काल, वस्तु तीनों के रग-रग में जो ओत-प्रोत है, जिसमें देश, काल, वस्तु है, जिस करके देश, काल, वस्तु हैं अथवा जो स्वयं देश, काल, वस्तु है तथा जो जिसमें सर्व है, जिससे सर्व है, जिस करके सर्व है और जो स्वयं सर्व है ऐसे भगवान सर्वात्मा का जो विधान यानी 'वासुदेवेद् सर्वं' यही समस्त चराचर विश्व का धर्म है। अरे भाई! जो जिसकी स्वाभाविक धारणा होती है वही उसका वास्तविक धर्म होता है। प्रत्येक हृदय की धारणा, जबकि नित्यानन्द है यानी दूसरे शब्दों में प्रत्येक का धर्म आत्म धर्म है, तब बाह्य धर्मों से विश्व के चित्त का समाधान कैसे हो सकता है? नदियों के चित्त का समाधान तो सागर पाकर ही होगा। इसी प्रकार जीव मात्र को तो संतुष्टि आनन्द सागर भगवान आत्मा को प्राप्त करने पर ही होगी।
वर्तमान काल की दशा पर जरा विचार करो। दवा ज्यों-ज्यों किया मर्ज बढ़ता ही गया।
सरिता जल-जल निधि महूं जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ।।
(रा.मा.कि.कां.)
आज जमाने में अनैतिक कार्यों का नाश करने के लिए रोज ब रोज नये-नये कानून बनते रहते हैं, परन्तु यह कोई नहीं विचार करता कि ये कानून किस पर लागू होंगे, शरीर पर अथवा हृदय परा अरे भाई! जो चीज जहाँ पर पैदा होती है, वहाँ का ही शासकीय विधान उस पर लागू होता है। अब विचार यह करना है कि जितनी भी नैतिक-अनैतिक भावनाएँ पैदा होती हैं, वे सभी शरीर से होती हैं अथवा हृदय से। समाधान यह है कि हृदय से ही पैदा होती हैं, न कि शरीर से। तब यह नियम है कि शरीर जिस देश का होगा, उसी देश का राजकीय विधान शरीर पर लागू होता है और हृदय किसी देश अथवा लोक-लोकान्तर का नहीं है। इसलिए हृदय पर किसी भी देश की गहर्नमेंट का कानून नहीं लागू हो सकता, तो भला बताओ कि बाह्य जगत् के शासकीय विधान से हृदय का सुधार या परिवर्तन कैसे हो सकता है? अब प्रश्न होता है कि फिर यह हृदय किस देश में पैदा हुआ अथवा किस देश का है और कौन-सा शासक है या इस हृदय पर किसका शासन है? समाधान यह है कि हृदय का शासक आत्मा है-आत्मा ही इस पर शासन करती है।
ईश्वरः सर्व भूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन् सर्व भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥
(गीता 18/61)
इसलिए, हृदय नारायण व्यापक तत्व जो सारे चराचर का अस्तित्व है और 'मैं' नाम से प्रत्येक काल, प्रत्येक अवस्था में प्रस्फुटित, प्रस्फुरित अथवा अभिव्यक्त हो रहा है, जिस भगवान आत्मा गह्वर्नमेंट का विधान हृदय पर लागू होता है, उसी व्यापक सरकार का ही कानून हृदय का परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा जितने भी विधान हैं, हृदय के बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए, जमाने को बदलने के लिए विश्व के कोने- कोने में अध्यात्मिक क्रान्ति की आवश्यकता है। नये युग का निर्माण करने के लिए कोई आसमान से नहीं आता, तुम स्वयं निर्माता हो, परन्तु भगवान के विधान पर अटल विश्वास करो। मन-मंदिर के अंदर विधान की स्थापना करो और इसी वैधानिक नियम के साँचे में अपने मानव-जीवन को ढालो। यही मानवता है, यही मानव धर्म, भगवद् धर्म एवं विश्व धर्म है। इस धर्म का संसार में कोई भी विरोधी नहीं है, क्योकि नित्यानन्द तो सभी चाहते हैं और दूसरे शब्दों में इसी को सनातन धर्म भी कहते हैं। यह धर्म विश्व के समस्त धर्मों का पिता है। आज जगत् में जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के प्रवर्तक तथा धर्मों की जन्म कुण्डली है, परन्तु माँ का कोई सपूत मैदान में आकर बतला सकता है कि सनातन धर्म का आचार्य कौन हुआ और सनातन धर्म किस सन्-संवत् में पैदा हुआ। इसलिए यह धर्म अनादि है, था और रहेगा। यद्यपि, इस धर्म पर बड़ी से बड़ी आपत्तियाँ आयीं, किन्तु कालांतर में उनका नामो निशां भी न रहा और यह धर्म अक्षुण ही रहा। सनातन धर्म को छोड़कर कोई भी यदि श्रुति-स्मृति के विरुद्ध, धर्म का आश्रय लेता है तो वह सनातन धर्म के स्वरूप को नहीं जानता। जिस प्रकार सम्राट के अंगरक्षक होते हैं, तद्वत् भगवान सनातन धर्म सम्राट के वेद से आदि हनुमान चालीसा तक अंग रक्षक हैं। यह धर्म महान है और इस धर्म की महत्ता यह है कि यह धर्म अन्य धर्मों का खण्डन नहीं करता, किसी की आलोचना नहीं करता, क्योकि सबका मूल कारण है, सबका आधार है। पुत्र भले ही पिता का विरोध करे, परन्तु पिता तो पुत्र का हित ही चाहता है। सनातन धर्म नारायण स्वरूप है और नारायण भगवान सारे चराचर की आत्मा हैं, फिर विरोध किससे? विरोध तो दो में होता है, जब एक ही आत्म तत्व बाहर-भीतर परिपूर्ण है, तब निंदा-स्तुति किसकी, राग-द्वेष किससे, तू-तू और मैं-मैं कहाँ? ऐसे विराद् धर्म का बिना अवलम्बन किये किसी भी क्षेत्र का अभिशाप अथवा गलित कोढ़ कभी मिट नहीं सकता। आसमान के सितारे भले ही जमीन पर आ जाएँ, विश्व हृदय का सुधार होना नितांत असंभव है। सत्य, सनातन, अजन्मा का जन्म, अजन्मा धर्म की ही रक्षा के निमित्त होता है और इसी धर्म के प्रसार के लिए सन्त रूप भगवद् विभूतियों का आविर्भाव समय-समय पर होता रहता है।
यतोऽभ्युदय निश्रेयस सिद्धिः स धर्मः ॥
(सांख्य दर्शन, भगवान कपिल)
जिससे कल्याण का उदय हो अथवा जिससे कल्याण पद की सिद्धि हो, वही धर्म है।
20. जगत् का स्वरूप
आँख बन्द करना है तो दिखने वाले से बन्द मत करो। क्योकि जो कुछ भी बाहर-भीतर दिख रहा है, सबको अपना स्वरूप भगवान आत्मा जानो, बल्कि यह अमुक है ऐसा मत मानो। इस प्रकार मानना ही संसार है और अमुक ही विकल्प है। विकल्प का अर्थ होता है कल्पना, यानी कहने सुनने में आये, परन्तु यदि निश्चय करने चलो तो उस पदार्थ की गंध भी नहीं, इसलिए विकल्प से आँख बन्द करो। जितने विकार अथवा उपाधियाँ है विकल्प जगत् में ही हैं। आत्म जगत् में तो मैं ही मैं जानो। इस अध्यात्म जीवन को हमेशा जीवित रखने के लिए वैकल्पिक जगत् की उपेक्षा करो। सबसे प्रथम अपने आप 'मैं' आत्मा में जीव या मन का विकल्प होता है। बाद में पंच महाभूत, दसों इन्द्रियाँ, शब्दादिक विषय, चतुष्टय अन्तःकरण, पंच प्राण, पंच कोषादिक, जायत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थायें, भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों काल, सारांश यह है कि जहाँ तक मन वाणी का विषय है वह सभी विकल्प अथवा अमुक जगत् है। जो दिखता है वह ईश्वर जगत् है और यह अमुक है ऐसा जो विकल्प है, वह जीव जगत् है। ईश्वर जगत् एक होता है, जीव जगत् अनेक होते हैं। स्वरूप ज्ञान होने पर वैकल्पिक (जीव) जगत् का नाश होता है, ईश्वर जगत् का नहीं। ईश्वर जगत् अहं रूप है, जीव जगत् इदं रूप है।
दिखने वाले को मन पहले कुछ मान लेता है, फिर माने हुए विषय में जाता है और अपने ही आनंद को उस विषय का आनंद मानकर उसमें आसक्त होता है। जिस समय अपने आप मैं को 'मैं' ही जानता है, उसी समय मन सहित सारा प्रपंच विलीन हो जाता है। फिर पता भी नहीं लगता कि कहाँ गया। मन अथवा जीव ये दो पदार्थ नहीं हैं, एक ही पहलू के दो नाम हैं-जीव या मन। सुषुप्ति अवस्था में मन के अभाव में जीव भाव का ही अभाव हो जाता है यानी मैं जीव हूँ, यह भाव नहीं रहता, परन्तु 'मैं' आत्मा रहता हूँ। यदि मैं न रहूँ तो आनन्द का अनुभव कौन करेगा? भगवान विश्वात्मा 'मैं' का कैसा खेल है? जब भगवान को खेलने की इच्छा होती है, तब अपने आपको कुछ भी मान लेता है और जब खेल बिगाड़ना चाहता है तब मैं को मैं ही जानता है, उस समय सारे खेल-तमाशे का अत्यंतप्रलय हो जाता है। आहा, मस्ती का दरिया उमड़ रहा है। मार दो छलांग, बहा दो साढ़े तीन हाथ की हस्ती को। मैं अमुक हूँ, इस अहंकार रूपी, नमक की पुतली को गला दो आनन्द सागर में। जीव-ब्रह्म, भक्त-भगवान, गुरु-शिष्य इत्यादि भावों को अभाव रूपी गठरी में बाँधकर फेंक दो चैतन्याकाश अपार समुद्र में। दरिया सीमा तोड़ कर बह रहा है। दोनों आँखों रूपी किनारों के बाहर बहने लग गया है। इस दरिया के बहने का रास्ता हद-बेहद से परे है। इस दरिया की आखिरी मंजिल कोई नहीं है। इस दरिया की न शुरुआत है, न आखिर है, लबालब है। क्या कहना, क्या सुनना, क्या लिखना, क्या पढ़ना? होश का पता नहीं, बेहोशी से नाता नहीं, खुदी की खुदकुशी है, चारों तरफ खामोशी है।
21. पेंसिल की लकीर
बोध बिना ध्यान, धारणा आदि पेंसिल की लकीर है अर्थात् जब तक अपने स्वरूप आत्मा 'मैं' का बोध नहीं हो जाता तब तक साधक जो कुछ भी साधन करता है, वह सब पेंसिल की लकीर के समान है। जिस प्रकार पेंसिल से लकीर खींचकर और फिर उसको रबर से मिटा सकते हो, इसी प्रकार किसी के बताने से अथवा मन को मानने पर जो कुछ भी ध्यान-धारणा इत्यादि साधन किये जाते हैं, वे सभी कल्पित हैं, क्योकि मन का माना हुआ हमेशा ही बनता-बिगड़ता रहता है। किसी के कहने से कोई साधन कर रहा है, किसी दूसरे ने कुछ और बता दिया तो पहले को छोड़कर दूसरा साधन करने लग गया। फिर उसको छोड़कर तीसरा, तीसरे को छोड़कर चौथा। बस, इसी में सारा जीवन समाप्त हो जाता है। चित्त को शान्ति नहीं मिलती और जहाँ तक साधन का प्रश्न है, वे सभी मन से मानकर और मन के ही लिए किये जाते हैं, परन्तु जो 'मैं' आत्मा है, यह मानने की चीज नहीं है, यह जानने की चीज है। मानना मन का धर्म है, जानना 'मैं' आत्मा का धर्म है और सारा प्रपंच ही माना हुआ है। जो पदार्थ माना जाता है वह कभी सत्य नहीं होता। वह असत्य, मिथ्या, कल्पित तथा बनने बिगड़ने वाला होता है और जो 'मैं' आत्मा है, उसको मानो तब है, न मानो तब है। जानो या न जानो, देखो या न देखो, ध्यान करो या न करो, धारणा करो या न करो, समाधि में बैठो या न बैठो। 'मैं' तो हर हालत में, हर काल में, हर अवस्था में सर्वत्र सर्व का सर्व भरपूर है, इसलिए अपने 'मैं' में सुख तथा शान्ति है, बाकी सभी में धोखा है।
भगवान को कुछ मानने से 'मैं' का कुछ नहीं बिगड़ता, 'मैं' को कुछ भी मानने से भगवान कलंकित हो जाता है।
अर्थात् भगवान को कुछ मानने से 'मैं' का इसलिए कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि मैं ही भगवान को मानता हूँ। मैं ही तो भगवान को सिद्ध करता हूँ। भगवान से 'मैं'को निकाल लो तो भगवान की भी हस्ती मिट जायेगी। इसलिए भगवान को कुछ मानने से 'मैं' का क्या बनना-बिगड़ना है, क्योकि 'मैं' तो सर्व का सर्व है।
22. श्रीमद्भागवतगीतासार
1. अर्जुन तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न जन्मती है, न मरती है।
2. जो कुछ हुआ सो अच्छा हुआ, जो कुछ होगा सो अच्छा होगा, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। भूतकाल का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल ही रहा है।
3. तुम्हारा क्या गया जो रोते हो। तुम क्या लाये थे, जो खो दिया। तुमने क्या पैदा किया, जो नाश हो गया। जो लाये हो और जो लिया, यहीं से लिया। जो दिया, यहीं पर दिया। जो लिया, इसी से लिया। जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आये और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसको तुम अपना समझकर मग्न होते हो, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुःख का कारण है।
4. परिवर्तन संसार का प्राण है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो यही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बनते हो और क्षण में कंगाल हो जाते हो। मैं-मेरा, छोटा-बड़ा, अपना पराया, दिल से हटा दो-विचार से मिटा दो फिर सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो।
5. यह देह न तुम्हारी है, न तुम इसके हो। देह-आग, पानी, हवा, मिट्टी से बनी है, इसी में मिल जायेगी। फिर भी तुम्हारा अस्तित्व स्थिर रहेगा, विचार करो तुम कौन हो?
6. तुम अपने आपको उसे समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह शोक, मोह, भय, चिंता से मुक्त रहता है।
23. वेदान्त क्या करता है?
प्रथम सूत्र-
वेदान्त हमें अमर बनना सिखाता है। मरना नहीं, वह मृत्यु को मार डालता है।
द्वितीय सूत्र-
वेदान्त उत्साह और उल्लास बढ़ाता है तथा सत्कर्म में प्रवृत्त करता है। वह आलस्य, विषाद और बुरे कर्मों की प्रवृत्ति को नष्ट कर डालता है।
तृतीय सूत्र-
वेदान्त विश्व के सब प्राणियों में एक अमर-आत्मा के दर्शन कराकर सबमें प्रेम कराता है। वह घृणा, द्वेष, बैर, परायेपन को मिटा देता है।
चतुर्थ सूत्र-
वेदान्त सारे संसार को सत्, चित् और आनन्द बनाकर दिखा देता है, वह जड़ता को सर्वथा नष्ट कर डालता है।
पंचम सूत्र-
वेदान्त कड़वी और दुःखभरी दुनियाँ को परम-मधुर, अतुल सुख से पूर्ण बना देता है। वह कटुता और कष्ट की जड़ ही काट डालता है।
षष्टम सूत्र-
वेदान्त जीवन को संयमी, संतोषी, निरहंकारी और कर्त्तव्यशील बनाता है। वह विषय-वासना, अतृप्ति, अहंकार और अकर्मण्यता को आमूल मिटा देता है।
सप्तम सूत्र-
वेदान्त हमारे जीवन को आत्मा या परमात्मा के परायण बना देता है। वह हमारी काम, क्रोध और लोभ परायणता को समूल नष्ट कर देता है।
अष्टम सूत्र-
वेदान्त ज्ञान की अप्रतिम, अपूर्व ज्योति जलाकर सर्वत्र निर्मूल एक रस अनन्त प्रकाश फैला देता है। वह अज्ञान के अंधकार को सदा के लिए मिटा देता है।
नवम सूत्र-
वेदान्त ऊँच-नीच के लौकिक व्यवहार के रहते हुए भी, आंतरिक ऊँच-नीच के भाव को सर्वथा मिटा देता है। वह उपाधि के कल्पित भ्रम भेद से हटाकर, हमें सर्वत्र नित्य अभेद स्वरूप सम ब्रह्म के दर्शन करा देता है।
दशम सूत्र-
वेदान्त मोह के सब पर्दों को फाड़कर, जीव की अपूर्ण साध को पूर्ण कर, उसे परमात्मा बना देता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता।
24. विद्या कल्पलता है
विद्या क्या करती है -
माता के समान रक्षा करती है। पिता के समान हित चाहती है। पत्नी के समान सुख-दुःख में साथ देती है और देश-विदेश में कीर्ति का प्रसार करती है।
विद्या क्या करती है -
देश-काल के अनुसार धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पदार्थ को प्राप्त कराती है।
विद्या क्या करती है -
अनैतिक मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लौटाकर, नैतिक पथ पर अग्रसर करती है।
विद्या क्या करती है -
समाज के पतन रूप अभिशाप को दूर कर, उत्थान रूप वरदान को प्रदान करती है।
विद्या क्या करती है -
मूढ़ को बुद्धिमान, निरक्षर को विद्वान, चरित्रहीन को चरित्रवान, असत्यवादी को सत्यवान, उद्दण्ड को नम्रशील, अनुशासनहीन को अनुशासित तथा कलंकी को निष्कलंक बनाती है।
विद्या क्या करती है -
आलस्य और प्रमाद को दूर कर, नैष्कर्मण्यता को मिटाकर, चित्त में उत्साह पैदाकर, कर्त्तव्यशील बनाती है।
विद्या क्या करती है -
मन, वचन, कर्म तीनों से एकत्व भाव का उपदेश करती है। यानी जो मन में हो, वही मुख से कहो और जो कहो उसे करके दिखाओ।
विद्या क्या करती है -
मानव जीवन रूप पहेली को सुलझाने में भली-भाँति सहायक बनती है।
विद्या क्या करती है -
किंकर्तव्यविमूढ़ व्यक्ति को आलोक में पहुँचाकर, अध्यात्म पथ का पथिक बनाती है।
शिव !!!
25. सत् चित् आनन्द
1. जिसमें संदेह नहीं वह सत् है। जिसमें अज्ञान नहीं वह चित् है। जिसका कोई विरोधी नहीं वह आनन्द है।
2. 'भास है' यही तो सत् है। भासना यही तो चित् है। इस भास से जो आनन्द, यही तो आनन्द है।
3. जो था, जो है और जो रहेगा वह सत् है। इसको जो जानता है, वह चित् है। जिसके लिए जो जाना जाय वह आनन्द है।
4. जिसमें शंका न हो वह सत् है। जिसमें अज्ञान न हो वह चित् है। जिससे वैराग्य न हो वह आनन्द है।
5. 'मैं' हूँ इसमें शंका नहीं, इसलिए 'मैं' आत्मा सत् हूँ।
'मैं' हूँ इसका अज्ञान नहीं, इसलिए 'मैं' आत्मा चित् हूँ।
'मैं' हूँ इससे वैराग्य नहीं, इसलिए 'मैं' आत्मा आनन्द स्वरूप हूँ।
6. सभी की इच्छा रहती है कि मैं हमेशा जीवित रहूँ, इसलिए जीव सत् है। सबों की यही इच्छा होती है कि मैं सब कुछ जान लूं, इसलिए जीव चित् है।
सबकी यही इच्छा होती है कि मैं हमेशा सुखी रहूँ, इसलिए जीव आनन्द स्वरूप है। कोई भी बंधन में एक सेकण्ड भी नहीं रहना चाहता, क्योकि जीव स्वतंत्र है।
छोटा बालक भी यही चाहता है कि घर के सभी छोटे-बड़े मेरे शासन में रहें, इसलिए जीव सबका शासक है।
26. कर्त्ता-कर्म-क्रिया
1. कर्म 4 प्रकार के होते हैं-
पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य-पाप मिश्रित कर्म और पुण्य-पाप रहित कर्म ।
लज्जा भय से रहित पुण्य कर्मी ला भय के सहित पाप कर्म। अपराधी को दण्ड देना पुण्य, संकोच भय के कारण दण्ड ना देना पाप, दोनों से संयुक्त पुण्य-पाप मिश्रित कर्म।
पुण्य और पाप दोनों विकल्प के अभाव में जो कर्म किये जायें उन्हें पुण्य-पाप से रहित कर्म कहते हैं।
2. भगवान के लिए वही कर्म, कर्म है, जो अर्थ रहित हो।
3. अर्थ रहित जो कर्म होते हैं, उन कर्मों का ही नाम पुण्य-पाप रहित कर्म है।
4. अर्थ रहित कर्म का अर्थ सहज कर्म होता है, क्योंकि भगवान सहज रूप है।
5. पुण्य-पाप कर्मों के अस्तित्व का अभाव ही ज्ञानाग्नि से कर्मों का दग्ध होना है।
6. पुण्य है, पाप है इस प्रकार का विकल्प कर्मों का अस्तित्व है।
7. बोधवान से अर्थहीन कर्म होते हैं। अज्ञानी से अर्थ सहित कर्म होते हैं।
8. आत्म देश में अर्थहीन कर्म होते हैं। जीव देश में अर्थ सहित कर्म होते हैं।
१. अत्यन्ताभाव जगत् में पुण्य-पाप दोनों कर्मों से रहित कर्म होते हैं।
10. ज्ञान जगत् में प्रारब्ध कर्म शेष रह जाता है, लेकिन 'मैं' आत्म जगत् में प्रारब्ध कर्म का भी नाश हो जाता है।
11. देह के अस्तित्व में प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व है। प्रारब्ध कर्म मानने तक अज्ञान का अस्तित्व है।
12. संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण ये कर्म है ही नहीं, इस प्रकार के अनुभव का नाम समस्त कर्मों का नाश है।
13. जो भास रहा है यह अकर्म रूप जगत् है और अमुक भास रहा है यह कर्म रूप जगत् है।
14. स्वाभाविक कर्म, अकर्म है। अस्वाभाविक कर्म, कर्म है।
15. कर्मों का विकल्प कर्मों का भाव है। विकल्प का अभाव सर्व का स्वभाव है।
16. अहंकार युक्त जो कर्म किया जाता है उसी की ही स्मृति रहती है। स्वभाव में स्थित होकर जो कर्म किया जाता है उसकी स्मृति नहीं रहती।
17. कर्मों के कर्त्तापने का अहंकार ही कर्मों का स्वरूप है।
27. मन (चित्त)
1. मन कैसा है? जैसा मैं मानता हूँ, वैसा ही मन है।
2. मन कहाँ है? जहाँ मैं हूँ।
3. मन कौन है? मन, मन है।
4. अपने आपको कुछ मानना ही मन की उत्पति है।
5. 'मैं' आत्मा को कुछ भी मान लेना ही मन का स्वरूप है।
6. न मन चंचल है, न स्थिर है। चंचलता का विकल्प ही चंचलता है, स्थिरता का विकल्प ही स्थिरता है।
7. मन का स्वभाव यदि चंचल है तो चंचलता का विरोध करना मानो खतरा मोल लेना है।
8. जब मैं कुछ बनता हूँ तब मन बनता है, जब में कुछ नहीं बनता तब मन भी नहीं बनता। अतः कुछ भी मत बनो।
9. अपने आप 'मैं' को जब तक कुछ भी माना जाय तब तक मन रूपी दाना कच्चा है। मैं को 'मैं' ही जानने पर इस ज्ञान रूपी अठिन में मज रूपी दाना भुन जाता है।
10. मन अर्थ में जाता है, पदार्थ में नहीं।
11. मन का विचरण मान्यता जगत् में है, आत्म जगत् में नहीं।
12. मन अविद्या जाल में फँसता है, विद्या में नहीं।
13. मन जीव सृष्टि में जाता है, ईश्वर सृष्टि में नहीं।
14. मन शुद्ध है तो 'मैं' ही हूँ और अशुद्ध है तो मन है।
15. मन को रोकने में जीव-भाव निहित है और न रोकने में 'मैं' भाव जिहित
16. मन को रोकने में चंचलता निहित है और न रोकने में स्थिरता निहित है।
17. मन के उदय में प्रपंच का उदय है और मन के अनुदय में प्रपंच का अनुदय है।
18. मन रोकने से नहीं रुकता, न रोकने से रुकता है।
19. कुछ बनने पर यह मन रोकने पर भी नहीं रुकता, लेकिन कुछ न बनने पर यह मन बिना रोके ही रुक जाता है।
20. मन के रोकने का प्रयास मन के रुकने में बाधक है।
21. मन को रोकने का प्रयास मन के अस्तित्व का पोषक है।
22. मन रोको मत, जाने दो।
23. रोकना है तो रोकने को रोको। जाने देना है तो जाने देने को जाने दो।
24. मन रोकने से रुकता है, न रोकने से स्थिर होता है।
25. मन के रुकने में भय है, स्थिर में निर्भयता है।
26. मन को स्थिर करना है तो मत रोको और मन को चंचल करना है तो रोको।
27. जो जिसकी वस्तु है उसकी स्थिरता उसी में होती है, अन्य में नहीं।
28. प्रत्येक विषय का अनुभव करने के लिए यदि मन उपकरण है तो सर्वकाल में मन स्थिर है। हाँ, यह भाव स्थिर नहीं अस्थिर है।
29. यदि अपने मन को वश में करना चाहो तो अपने स्वरूप आत्मा से मन को अलग मत देखो।
30. अपने 'मैं' आत्मा को कुछ भी न मानने पर ही मन वश में होता है।
31. मन देश में खड़े होकर देखो तब मन का अस्तित्व है और स्वरूप स्थिति में स्थित होकर देखो तो मन तीन काल में है ही नहीं।
32. मन मारने का सबसे बड़ा हथियार यही है कि मन की हस्ती को न मानना।
33. जिस प्रकार भगवान की तलाश न करने पर भगवान मिलता है, इसी प्रकार मन को न रोकने पर मन रुकता है। विश्वास न होतो अनुभव करो।
34. मैं अमुक हूँ, इस भाव से मैं मन के बस में हो जाता हूँ और मैं 'मैं' हूँ इस भाव में मन 'मैं' के बस में हो जाता है।
35. मन द्वारा रचित भगवान, उसका भजन, मन की एकाग्रता पर निर्भर है, मन से परे जो भगवान उसके भजन के लिए एकाग्रता की उपेक्षा है।
36. भगवान का सर्वकालीन स्मरण वही है जो मन के भाव में भी हो और अभाव में भी हो। जब मन का स्वभाव ही चंचलता है तब निग्रह किं करिष्यति।
37. भगवान का स्मरण मन से नहीं होता।
38. मन जीतने की चीज नहीं है। मन जीतने के विकल्प के पीछे शत्रुता खड़ी है। जब मन को शत्रु मानते हो तभी जीतने का प्रश्न होता है।
39. जब मन भगवान से अलग नहीं है तो जीतोगे किसको।
40. भगवान और गुरु को अपना मन ही देना चाहिए, क्योंकि मन के सिवाय अपना कुछ है भी नहीं। स्त्री-पुत्रादिक अपने नहीं हैं।
41. आत्म कृपा से मन स्थिर होता है। संत कृपा से मन लय होता है।
42. कृत्रिम साधन काल में मन नारायण रूप नहीं जीव रूप रहता है, इसलिए मन को एकाय करने में कठिनाई पड़ती है।
43. मन स्वाभाविक एकाय हो जाने पर नारायण रूप रहता है और कृत्रिम साधन द्वारा मन एकाग्र होने पर जीव रूप हो जाता है।
44. हर समय हर अवस्था में मन नारायण ही है। इसलिए मन स्वाभाविक एकाग्र है।
45. मन 'स्व' के भाव में स्वभाव रहता है और 'पर' के भाव में मन हो जाता है।
46. तुम स्वभावी हो, मन तुम्हारा स्वभाव है।
47. मन स्वभाव होने के कारण स्वाभाविक रुकता है, साधन से नहीं रुकता।
48. मन में जो क्रियाशीलता भासती है, वह मन का स्वभाव है, मन का विकार नहीं।
49. आत्मा अकृत्रिम, अक्रिय है और मन आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव रूप मन अकृत्रिम, अक्रिय स्वभावी आत्मा से भिन्न नहीं है।
50. मन अकृत्रिम, अक्रिय आत्मा का है। इसलिए, काल्पनिक, कृत्रिम क्रिया रूप साधनों के द्वारा यह मन स्थाई एकाय नहीं हो सकता।
51. मन के भाव-अभाव के भाव का अभाव जिस देश में हो जाता है, वह 'मैं' हूँ।
52. मन के आने-जाने का अनुभव करना पदार्थ (आत्मा) का अनुभव करना है। मन के आने-जाने का विकल्प करना संसार का विकल्प करना है।
53. बाह्य तथा अन्तर्जगत के किसी भी विषय के अनुभव करने में मन की अपेक्षा नहीं है।
54. शब्दादिक विषयों के अनुभव काल में 'मैं' स्वभाव में स्थित रहता हूँ, इसलिए उस समय मन का अत्यन्ताभाव रहता है और पूजा-पाठ, ध्यान-धारणा इत्यादि के समय अपने-आपको संसारी जीव मानता हूँ, इसलिए उस समय मन का प्रादुर्भाव होता है।
55. पूजन-पाठ, ध्यान-धारणा ये सभी जीव देश के कार्य हैं, इसलिए इनमें मन का रोकना दुःसाध्य है।
56. संसार के प्रत्येक विषय के अनुभव काल में में 'मैं' रहता हूँ, इसलिए मन के आने-जाने में हर्ष-शोक नहीं होता और पूजा-पाठ, ध्यान- धारणा में जीव हो जाता हूँ, इसलिए मन काबू के बाहर हो जाता है।
57. किसी भी विषय के अनुभवकाल में मन रहता ही नहीं। यदि विषय के अनुभवकाल में मन रहेगा तो उसी तरह अड़चन होगी, जिस तरह पूजा-पाठ, ध्यान-धारणा के समय होती है।
58. स्वरूप की विमुखता में मन का अस्तित्व है और मन के अस्तित्व में एकाग्रता की कल्पना है।
59. मन के अस्तित्व में रोकने का विकल्प है। मन के अभाव में विकल्प का अभाव है।
60. मन के अस्तित्व में मेरा मन है और भगवान को दे दिया तो 'मैं' मन हूँ।
61. जब तक मन कहता है कि मैं मन हूँ तब तक डोलता है और जब मन कहता है कि 'मैं' आत्मा हूँ तब अडोला हो जाता है।
62. जब यह मन किसी भी विषय का विषय करता है तब इसका नाम हो जाता है मन और जब निर्विषय हो जाता है, तब इसका नाम हो जाता है भास (जगती) और भास है वही अभास (आत्मा) है।
63. जिस समय मन दुःख सुख रूप प्रतीत हो तो समझना कि मन सविषय है और जिस समय दुःख-सुख दोनों की प्रतीति न हो तो समझना कि मन निर्विषय है।
64. जिसे मन न छोड़े वही सुख है और जिससे मन भागे वहीं दुःख है।
65. सविषय मन, मन है और निर्विषय मन 'मैं' हूँ।
66. तमोगुणी मन में अपना स्वरूप साढ़े तीन हाथ का दिखता है। रजो- गुणी मन में अपना स्वरूप संसारी जीव दिखता है। सतोगुणी मन में अपना स्वरूप एक और व्यापक दिखता है और त्रिगुणात्मक मन के अस्तित्व के अभाव में मैं जैसा हूँ, वैसा ही दिखता हूँ।
67. आत्म देश में पहुँचने पर मन का अत्यन्ताभाव हो जाता है।
68. मन की विक्षेपावस्था एवं समाधि अवस्था की कल्पना का न उठना ही आत्मदेश का निवास है।
69. विषयों से मन रहित हो जाना ही ध्यान है।
70. मन के निरोध में प्राण का निरोध और प्राण के निरोध में मन का निरोध है। मन और प्राण के निरोध में वासना का निरोध और वासना के निरोध में मन और प्राण का निरोध है।
71. मन का प्रेम ब्रह्म से है न कि विषय से, क्योंकि दोनों ही नपुंसक लिंग हैं। ब्रह्म के समान मन भी अक्रिय है।
72. मन जब तक आत्मा नहीं होता तब तक उसका संकल्प सिद्ध नहीं होता।
73. मन के अत्यन्ताभाव का ही नाम मन का विलीनीकरण है।
74. मन के अस्तित्व के अभाव का भाव ही मन का विकेन्द्रीकरण है।
75. मन के तुम घर हो, मन की खुराक हो, मन के प्राण हो, मन के उत्पत्ति, *पालन, संहार का स्थान हो। तो फिर मन को आनन्द सागर अपना आप क्यों नहीं दे देते।
76. यदि मन तुमसे ही मिलने का इच्छुक है तो तुम आटमा मन को क्यों नहीं दर्शन दे देते।
77. यदि इस मन को तुम्हारी ही प्यास है तो तुम आनन्द स्वरूप उसमें क्यों नहीं समा जाते।
78. यदि तुम ही मन के घर हो तो आप से बाहर काल्पनिक पदार्थों में स्थिर करने की कोशिश क्यों करते हो।
79. यह मन क्षणिक आनंद में निरोध और एकाग्र होता है। नित्यानन्द में स्थिर और लय होता है।
80. मन का बहाव स्वाभाविक आनन्द की ओर है, न कि कृत्रिम की ओर।
81. मन के निरोध का फल विशेष आनंद है। मन के अनिरोध का फल सामान्य आनन्द है। विशेष आनन्द का पर्याय विषयानन्द या क्षणिक आनन्द और सामान्य आनन्द का पर्याय ब्रह्मानन्द, नित्यानन्द तथा आत्मानन्द है।
82. यदि मन चिंताओं से मुक्त है तो शरीर कभी रोगी नहीं हो सकता।
83. मन रोकने के विकल्प का अभाव ही मन के रोकने का अभ्यास है।
84. मन के अस्तित्व के त्याग का नाम वैराग्य है और मन, वचन, कर्म तीनों से कुछ भी साधन न करना ही अभ्यास है।
85. मन के रोकने का अभ्यास आत्म देश का प्रवास है।
86. मन के रोकने का अभ्यास आत्म देश का अस्थाई निवास है।
87. मन के न रोकने का अभ्यास स्वरूप स्थित नगर का स्थाई निवास है।
88. मन निरोध का अनभ्यास अंधे की जैसी टेढ़ी खीर है।
89. मन सदैव रुका है, इसकी अनुभूति ही मन के रोकने को रोकना है।
90. मन को न रोकना ही मन के रोकने का साधन है।
91. मन को मन न मानना ही मन की स्थिरता का साधन है।
92. मन की याद न करना ही मन के निरोध का साधन है।
93. स्व-स्वरूप में स्थित हो जाना ही मन के लय का साधन है।
94. मन को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का साधन न करना ही मन को रोकने का साधन है।
95. किसी भी देश में किसी भी वस्तु के साथ मन को बांध देने से मन का क्षणिक निरोध होता है।
96. मन की एकाग्रता कृत्रिम साधनों से क्षणिक होती है और स्वाभाविक स्मरण रूप साधन से मन स्थाई एकाय होता है।
97. काल्पनिक विषय में यह मन कृत्रिम साधन द्वारा क्षणिक एकाग होता है और स्वाभाविक विषय आत्म स्वरूप में यह मन स्वभावतः स्थाई रूप से एकाग होता है।
98. कृत्रिम साधन क्रिया रूप होता है और स्वाभाविक साधन अक्रिय होता है।
99. कृत्रिम साधन काल्पनिक होता है और अकृत्रिम साधन स्वाभाविक होता है।
100. मन को जीतना साधन का विषय नहीं है। मन की उपेक्षा करना मन के नाश का साधन है। अपने आपको देखना ही मन की उपेक्षा है।
101. मन है, यह मानकर मन के रोकने का साधन मत करो। मन नहीं है ऐसा जानकर साधन करो।
102. साधन काल तक मन रहता है। साधन समास हो जाने पर मन की समाप्ति हो जाती है।
103. मन की एकाग्रता और निरोध साधन जन्य है, स्थिर और लय कृपाजन्य है।
104. मन को अक्रिय बनाने के लिए मन, वचन, कर्म द्वारा कुछ भी साधन न करना ही परम साधन है।
105. जिस प्रकार स्वरूप स्थिति स्थिर है, इसी प्रकार मन की एकाग्रता भी स्थिर है।
106. मन को स्थिर करना चाहो तो अपने में को आत्मा जानो और यदि रोकना है तो जीव मानो।
107. मन अथवा माया ये दोनों ही आत्म स्वरूप हैं। व्यष्टि दृष्टि से मन और समष्टि दृष्टि से माया।
108. मन है तो माया है, मन नहीं तो माया नहीं।
109. यदि माया से तरने की इच्छा है तो माया पति को माया से भिन्न मटा जानो।
110. एक शरीर के अंदर की चंचलता का नाम मन है और समस्त शरीरों की चंचलता का नाम माया है।
111. आत्मबोध का फल चित्त का समाधान है।
112. चित्त का समाधान ही शिष्यत्व भाव का प्रतीक है।
113. चित्त कहता है कि मैं चित्त हूँ, इसलिए 'मैं' चित्त हूँ।
114. 'मैं' से भिन्न अगर चित्त है तो चित्त नहीं और अभिन्न है तो चित्त नहीं।
115. मन के निरोध में हो और अनिरोध में न हो, वह मन का ही चिंतन है और निरोध-अनिरोध दोनों में जो हो वह आत्म चिंतन है।
116. मन बनाकर चिंतन करना चित्त का चिंतन है। न बनकर, न बनाकर चिंतन करना चित (आत्मा) का चिंतन है।
117. चंचलता ही चित्त है और निश्चलता ही चित् है।
118. चित्त के चिंतन से चिंता का विकास है। चित् के चिंतन से चिंता का विनाश है।
119. विकल्प सहित निर्विकल्प चित्त है। निर्विकल्प के विकल्प का अभाव ही चित है।
120. निर्विकल्प चित्त, चित्त का विकार है। निर्विकल्प चित, चित का स्वभाव है।
121. निर्विकल्प चित्त में विकल्प का भय है। निर्विकल्प चित में भय का भी भय नहीं।
122.
चित ही चित्त, चित्त ही चित है। चित विज्ञापक, चित ही चित ॥
चित्त विकल्प, विकल्पक चित है। चित्त विवर्त, विवर्तक चित ।
चित है बिम्ब, चित्त प्रतिबिम्बित । चित सागर, आवर्त है चित्त ॥
चित्त अचित्य उभय तज, चित भज । चटपट हो, सब अन्टा चित ॥
28. लुधियाना स्मृति
उस स्थिति का अनुभव करो, जिसमें तुम हमेशा रहते हो। कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं कि स्वामीजी, जब तक आपके पास बैठे रहते हैं, तब तक तो बड़ा विलक्षण आनन्द आता है और जब घर चले जाते हैं तो पता नहीं आनन्द कहाँ चला जाता है। भैय्या ! आनन्द दो प्रकार का होता है। एक विशेष आनन्द और एक सामान्य आनन्द ! जिसका अनुभव मैं करता हूँ वो विशेष आनन्द है और जिसका अनुभव नहीं होता... वह सामान्य आनन्द है। जिसका अनुभव होता है, वह विशेष आनन्द है, मनोजन्य आनन्द है, मन की स्थिरता का आनन्द है, क्षणिक आनन्द है, अनित्य आनन्द है अथवा अनित्य सुख है अथवा दूसरे शब्दों में विषयानंद है, चाहे शब्दादिक विषयों के द्वारा आनन्द की उपलब्धि हो, प्राप्त हो अथवा समाधि के द्वारा आनन्द मिले, मगर है वह भी विषयानन्द। क्योकि समाधि नित्य तो होती ही नहीं। चाहे समाधि एक दिन की हो, एक कल्प की हो, एक युग की हो। समाधि जब तुमने लगाई है तो कभी न कभी टूटेगी ही...। तो, समाधि जन्य आनन्द को भी हम ब्रह्मानन्द नहीं कहेंगे। (मुक्तानुचर) शास्त्रीजी 'जी'। वह भी विषयानन्द ही है। और फिर, उसका अनुभव भी मैं करता हूँ। वाह बड़ा मजा आया। बड़ा आनन्द आया। ये विषयानन्द है। जिस आनन्द को मैं जानता हूँ। जिस सुख का अनुभव मैं करता हूँ वो आत्म-सुख नहीं है, विषयानन्द है। और, जहाँ पर सुख और दुःख की अनुभूति नहीं होती वो ब्रह्म सुख है। वाह! 'मैं' आत्मा!
(मुक्तानुचर) शास्त्रीजी -
शोक, मोह, भय, हरष, दिवस, निसि, देस, काल जहं नाही।
सुख-दुःख से कोई परे परमपद तेहि पद रहा समाई ।।
गरज ये है कि अभी जो ये सुन रहे हो (हमसे जो सुन रहे हो) ये भी एक विषय है। और, इस विषय के श्रवण काल में चित्त का निरोध होता है। जी। तो वृत्तिजन्य आनन्द को विशेष आनन्द कहते हैं। यह ही तुमको यहाँ सामने मिलता है। और, जब घर जाते हो तो यह विषय नहीं रहता। तो आनन्द भी नहीं मिलता तो तुम घबरा जाते हो। नहीं गा? जी! बिल्कुल ठीक !! भइगे महराज ! एक रस स्थिति हमारी नहीं रहती। अरे, स्थिति भी कभी एक रस रहती है। जो स्थिति बनी है भैय्या, वो एक रस कैसे रहेगी। उस स्थिति और अस्थिति का जो अनुभव करता है, जानता है वो 'मैं' आत्मा एक रस हूँ। बाकी स्थिति तो बनती बिगड़ती रहती है, जी हाँ! वाह ! शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, ये सब क्षणिक सुख के साधन हैं। इन विषयों के द्वारा जो क्षणिक आनन्द प्राप्त होता है, उसमें मन विभोर हो जाता है और उसी को स्थिति समझ के उसी में लट्टू हो जाते हैं और जब वह विषय नहीं रहा तो विषय के अभाव में (विषयजन्य सुख का भी अभाव हो जाने पर) वो व्यक्ति घबरा जाता है कि हमारी स्थिति कहाँ चली गयी। अरे, गयी कहाँ? वाह! मैं तो उस स्थिति का जानने वाला, जहाँ का तहाँ हूँ। वहीं का वहीं हूँ जिस सुख को पाकर मन सुखी होता है, वह विषयजन्य सुख है और जिस सुख को पाकर मन अमन हो जाता है वह ब्रह्म सुख है (मुक्तानुचर) 'जी', जिस सुख को पाकर मन अमन हो जाता है, भगवान हो जाता है, मन आत्मा हो जाता है, वह ब्रह्म सुख है। वह आत्म सुख है। वह निज सुख है। तो स्त्री- पुत्र कलत्रादि साधनों के द्वारा जो... स्त्री-पुत्र कलत्रादि इत्यादि का परित्याग करके पूजा-पाठ, ध्यान-धारणा में जो सुख मिलता है, इस सुख में और प्रपंचजन्य सुख में कोई अंतर नहीं है। कोई साधन तमोगुणजन्य है, कोई रजोगुण और कोई साधन सतोगुणजन्य है। ध्यान-धारणा, समाधि सतोगुणजन्य साधन है, विषयादिक प्रपंच तमोगुण, रजोगुणजन्य हैं। मगर सुख तो एक ही है। मगर इनको जो जानता है, इनका जो अनुभव करता है वह 'मैं' आत्मा...। वाह! इसी स्थिति में तुम हमेशा रहते हो। सुख को छोड़ दो, दुःख को छोड़ दो-यही हमेशा रहने वाली स्थिति है। इस स्थिति से कभी कोई विचलित नहीं रहता। तुम जानो तब ये स्थिति है तुम्हारी, न जानो तब ये स्थिति है। इससे तुम कभी विचलित नहीं होते। इससे तुम कभी टस से मस नहीं होते। ऐसी स्थिति का अनुभव करो, जिसमें तुम हमेशा रहते हो। वो हमेशा रहने वाली जो स्थिति है, वो साधनजन्य नहीं है। संतशरण की देन कहो अथवा संतकृपा। इसी को सहजपद, सहजावस्था। बिना कुछ किये ही जो प्राप्त हो-वह सहज है। भगवान का विशेषण शास्त्रों में, रामायण में...
सहज पद -
सहजहिं चले, राम भगवाना । सहज प्रकाश, रूप भगवाना ||
संकर सहज, स्वरूप संभारा । सहज स्नेह, स्वामी सेवकाई ।।
क्योकि परमात्मा सहज है, जो सर्व का अपना आप होता है। यही स्थिति हमेशा रहने वाली स्थिति है। ये स्थिति बनाए से नहीं बनती और न इसके लिए कोई साधन है। स्थिति तो स्वयं ही है। संत महानपुरुष कृपा करके उसकी अनुभूति करा देते हैं। स्थिति में स्थित नहीं करते, स्थिति की अनुभूति करा देते हैं। उस स्थिति का अनुभव करो। कौन सी? उस स्थिति का। ये संकेत किधर जा रहा है। उस स्थिति का...। जिस स्थिति में तुम हमेशा रहते हो। इतना ही संकेत किया जा सकता है, जिसमें तुम हमेशा रहते हो। अब 'मैं' किसमें हमेशा रहता हूँ? किसी के ध्यान में रहता हूँ कि किसी की धारणा में रहता हूँ कि किसी की समाधि में रहता हूँ कि किसी के राग में रहता हूँ कि किसी के द्वेष में रहता हूँ। किसमें 'मैं' हमेशा रहता हूँ। कौन सी स्थिति है? वाह! अरे उस स्थिति में 'मैं' हमेशा रहता हूँ, जिस स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति है ही नहीं। शिव! उस स्थिति में 'मैं' हमेशा रहता हूँ, जिस स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति है ही नहीं। अब किसी को मत बाँधो, किसी को मत रोको। बिना रोके, बिना बांधे अगर मन बंध जाय, बिना रोके मन रुक जाय, बिना रोके इन्द्रियाँ कहीं न जायें तब समझ लेना कि यही हमेशा रहने वाली स्थिति है। अरे, जिस स्थिति का अनुभव कर लेने पर... शिव! जिस स्थिति में रहने पर (ऐसा कहो) उस स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव न हो... वही हमेशा रहने वाली स्थिति है। (ऐसा कहो) याद दिला दो, हम क्या कह गए हमको याद नहीं। जिस स्थिति में रहने पर उस स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव न हो-वही हमेशा रहने वाली स्थिति है। वाह! अब बिल्कुल साफ हो गया। क्लीयर...। (जी भैय्या! ये सब नोट ले लेना। जरा जरा सी हिंट) फिर से कहो क्या कहा मैंने। जिस स्थिति में रहने पर उस स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव न हो, वही हमेशा रहने वाली स्थिति है। ये बात...। अब पकड़ लो इसको, अभी इसके ऊपर कुछ अनुभव करायेंगे। जमा लो ! अभी चर्चा हो रही है जिसकी, बड़ी विलक्षण चीज है। जिस स्थिति में रहने पर स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति नहीं रहती यही हमेशा रहने वाली स्थिति है। याने हाँ देखो-जिस स्थिति में रहने पर उसके सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव न हो वही हमेशा रहने वाली स्थिति है। 'वाह।' घूम गया दिमाग! अब समझो इसको - अब जमो इसमें ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित है या अहंकार है, ये इन्द्रियाँ हैं, ये प्राण हैं। में रत्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं जड़ हूँ या चेतन हूँ, मैं सत्य हूँ या असत्य हूँ या 'मैं' हूँ कि वह हूँ।
(मुक्तानुचर शास्त्रीजी) - कि 'तू' है कुछ भी अनुभव न हो। स्वामी जी-क्या हमेशा इन स्थितियों का अनुभव होता है।
प्रतिमा बहन - कोई भी ऐसी चीज नहीं, जिसका अनुभव हमेशा रहता हो।
स्वामीजी- जब वो स्थिति दरअसल होय तब तो उसका अनुभव हो। वो स्थिति तो हमारे बनाए से बनती है। हाँ जी! जी हाँ! जब 'मैं' मानता हूँ मन तो मन बन जाता है, जब 'मैं' मानता हूँ बुद्धि तो बुद्धि आ जाती है। इन्द्रियाँ मानता हूँ तो इन्द्रियाँ आ जाती हैं। जब कोई पूछता है तो 'मैं' कहता हूँ और नहीं पूछता तो-जाव! देखो, किसी के न पूछने पर जो 'मैं' रहता हूँ, वही 'मैं' हूँ। किसी के न पूछने पर भी जो रहता हूँ...। वाह!
प्रतिमा बहन- अपने आपके न पूछने पर, न बनने पर जो रहता है।
स्वामी जी- शिव! क्या अकेले भी 'मैं' 'मैं' चिल्लाता हूँ?
प्रतिमा बहन- ना।
स्वामी जी- अगर अकेले में चिल्लाऊँ तब तो 'मैं' हूँ। अरे, सुषुप्ति में, समाधि में, मूर्छा में कहाँ 'मैं'- 'मैं' कहता हूँ। मगर रहता तो हूँ। उस स्थिति का अनुभव करो, जिसमें हमेशा रहते हो।
प्रतिमा बहन- स्वामी जी! शाल ओढ़ लो ठण्डी है।
स्वामीजी- फिर ये जो निरूपण हो रहा है, ये शाल से कम है? गनगना आती है...। तबीयत
प्रतिमा बहन- मेरा दिमाग गरम हो गया था, चक्कर हो गया था।
स्वामी जी-तुम ग्रहण कर रहे हो ना। ग्रहण-त्याग में ये सब बातें होती हैं। यहाँ ग्रहण-त्याग है ही नहीं।
प्रतिमा बहन - हे राम! जो कुछ होगा वो ग्रहण-त्याग तो नहीं है, लेकिन जो कुछ करना-धरना, वो काहे में रहेगा? सुबह-सुबह आप बता रहे थे ना कि हम भास-भास देख रहे हैं। आज सुबह ही।
स्वामीजी-ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, यह भी तो भास ही है। (हंस रहे हैं सभी) 'जी हाँ।' ये भी तो भास ही है।
प्रतिमा बहन- कह रहे थे सुबह-सुबह अर्थ नहीं है, अर्थ का भान नहीं होता। भास-भास हमको दिखाई देता है तो मैंने कहा- स्वामी जी-फिर मैंने सोचा कि नहीं बोलना चाहिए-चलना-फिरना, काम-धाम सब अर्थ में है कि भास में?
स्वामी जी- नहीं, देखो! देखो !! भास चौबीस घंटा रहता है। यही हमेशा रहने वाली स्थिति है। और, विकल्प तो कभी-कभी आता है। जिस स्थिति में रहने पर वैकल्पिक स्थितियों का अनुभव न हो, वही हमेशा रहने वाली स्थिति है।
प्रतिमा बहन- जिस स्थिति में रहने पर विकल्प होने वाली स्थिति में स्वामीजी-वैकल्पिक।
स्वामीजी - वैकल्पिक स्थितियों का अनुभव न हो, वही हमेशा रहने वाली स्थिति है। (मुक्तानुचर शास्त्रीजी) - अब स्वामी जी को मैं बोल रहा हूँ, ये अनुभव नहीं हो रहा है।
स्वामीजी - न, बिल्कुल न!! यही हमेशा रहने वाली स्थिति है। अगर अनुभव होगा तो मोर ददा नइ बोल सकय। हाँ। मैं बोल रहा हूँ ये अनुभव नहीं हो रहा है। यही हमेशा रहने वाली स्थिति है। हमी नहीं। 'जी नहीं!' ये सबकी बात है। जो कोई भी बोलता है, मैं बोल रहा हूँ, ये अनुभव नहीं होता। पशु-पक्षी, ज्ञानी-अज्ञानी, सबका यही हाल है। सत्, बिल्कुल ठीक है महराजा मुक्तानुचर शास्त्रीजी-किसी को अनुभव नहीं होता कि में बोल रहा हूँ। अच्छा! कर्म करता है, तब भी ये कर रहा हूँ, ये अनुभव नहीं होता।
प्रतिमा बहन- बोलता क्या, करता क्या, चलता क्या, जो कुछ भी करता है तो ये अनुभव थोड़े ही होता है।
स्वामी जी- जी हाँ! यही हमेशा रहने वाली स्थिति है।
झाडू दाऊ- अच्छा, वो निकालो ना सूत्र थोड़ा।
मुक्तानुचर शास्त्रीजी - रहौनगा, चलन दौ ना इही ला, राहन दौ ना इही ला जी ।
(रहने दो ,इसी को चलने दो, इसी को रहने दो)
स्वामी जी- उटकुटागे का गा? (ऊब गये क्या ?)
झाडूराम - नहीं, कापी ला निकालिस ना तब इही ला कहत रेहेंव। (नहीं डायरी को निकाले न इसलिए इसी को कह रहा हूँ ।)
मुक्तानुचर शास्त्रीजी- कई कोटि निकलही अभी। (कई कोटि निकलेगा अभी।)
स्वामी जी - वाह! उस स्थिति का अनुभव करो... यही हमेशा रहने वाली स्थिरता है। स्थिति और अस्थिति दोनों की अनुभूति, जिस स्थिति से होती है वही हमेशा रहने वाली स्थिति है। जैसे, सुन रहे हो विषय को हमसे।
मुक्तानुचर शास्त्रीजी-सुनने का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। स्वामी जी- 'जी।' जब कोई पूछता है, क्या कर रहे हो? तब उस वक्त फिर कर्ता, कर्म, क्रिया, तीनों बन जाते हैं। न दर्शन-काल में दृश्य का अनुभव होता है, न श्रवण क्रिया काल में शब्द विषय का अनुभव होता है? यही हालत है। ओ हो... प्रशान्त महासागर अपनी महिमा में ज्यों का त्यों स्थित है। वाह! अब छोड़ दो बागडोरा षण्डनपुंसक की बागडोर छोड़ दो।
स्वामी जी - प्रिंसिपाल साहब (ठा. जवाहर सिंह जी) नहीं रहे, जब गए थे स्टेशन। एक और अनुभव निकला था। 'जी' वही!
प्रिंसपल सा.- 'षण्ड नपुंसक' क्या है? मैं भी पूछने वाला था।
प्रश्न ये था कि मन कब पैदा होता है? किससे पैदा होता है? मन क्यों पैदा होता है? तो, जैसे प्रकृति-पुरुष के संयोग से संतान पैदा होती है, उसी तरह मान्यता जो है प्रकृति है और आत्मा जो है पुरुष। 'मैं' आत्मा पुरुष हूँ। जो मान्यता (प्रकृति) और चेतन 'मैं' आत्मा (पुरुष) दोनों के संयोग से मन रूपी लड़का पैदा होता है। हमेशा रहने वाली स्थिति में मन नहीं रहता। हाँ, उस समय मुण्डा नहीं रहता और न कुड़ी रहती। हमेशा रहने वाली स्थिति में मन नहीं रहता और मन के नहीं रहने पर कर्त्ता, कर्म, क्रिया। द्रष्टा, दर्शन, दृश्या ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। किसी की अनुभूति नहीं होती। और, जहाँ अपने 'मैं' को माना कि 'मैं' अमुक हूँ तो मान्यता और आत्मा दोनों का (जहाँ प्रकृति-पुरुष का) संयोग हुआ तो फट्ट से 'मुण्डा' पैदा हो गया।
मुक्तानुचर शास्त्री जी- 'जी।' स्वामी जी- यही मन की पैदाइश है। अब मन को व्याकरण शास्त्र में नपुंसक लिंङ्ग कहा है-मनः, मनसि, मनांसि और ब्रह्म भी नपुंसक लिङ्ग है-ब्रह्म, ब्रह्माणि, ब्रह्माणि तो कहते हैं कि शंका होती है कि नपुंसक से तो कुछ भी पैदा नहीं होता। वो तो हिजड़ा माना जाता है। और, हमेशा मायूसी रहती है चेहरे पर, सिवाय ताली बजाने के उससे कुछ नहीं होता। हिंजड़ा ताली बजाते हैं कि नहीं? मुक्तानुचर शास्त्रीजी- "जी।' स्वामी जी- और उनसे कुछ नहीं होता। तभी तो भीष्म दादा ने शिखण्डी के सामने रख दिया था धनुष-बाण। लो साले मारो। विश्व-विजयी योद्धा और हिजड़ा से लड़े। हाँ! ये मन जब नपुंसक लिंङ्ग है तो ये हिंजड़ा है और साले हिजड़ा में ताकत इतनी है कि क्या नाम से ये क्षण में हजारों ब्रह्मा बनाता बिगाड़ता है। बड़े-बड़े को उठा-उठा के पटकता है। हिंजड़े में ये ताकत क्यों आयी? ये शंका समझ में आ गयी। मुक्तानुचर शास्त्री जी- 'जी।' स्वामी जी-नपुंसक होते हुए भी। तो ये 'साला विपरीत मैथुन से पैदा हुआ है। 'मैं' पर मान्यता-मान्यता पर 'मैं' नहीं। आ गया समझ में? मुक्तानुचर शास्त्री जी- 'जी।' स्वामी जी-जान दे कहिथे भैय्या! तो उस स्थिति का अनुभव करो, जिसमें तुम हमेशा रहते हो।
मन ने माना जगत् को, मन को मान्यो आप ।
मन मिटते जग मिट गया, 'मुक्ता' गुरु परताप ।।
मैंने माना मन को और मन ने माना 'मैं' को। मुक्तानुचर शास्त्री जी- 'जी।' स्वामी जी- जब मैंने मन को माना तो फिर मन की सृष्टि शुरू हो गयी कि ये शरीर है, ये कर्त्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। ये द्रष्टा है, ये दर्शन है, ये दृश्य है। ये सभी मन के माने हुए हैं। नहीं तो हमेशा रहने वाली स्थिति तो है ही। किसी का भी अनुभव नहीं होता। कैसे स्वभाव में मस्त बैठे हो। अगर इस वक्त किसी भी व्यवहारिक जगत् के कार्य में मन चला भी जाता है तो, अरे, नहीं होता, ग्लानि नहीं होती कि क्यों गया और आ जाता है तो हर्ष नहीं होता। वाह! क्यों नहीं होता? क्योंकि 'मैं' उस स्थिति में स्थित रहता हूँ, जिसमें हमेशा रहता हूँ। हमेशा रहने वाली स्थिति में रहने पर मन के गमनागमन होने पर हर्ष-शोक नहीं होता। मुक्तानुचर शास्त्री जी- 'जी।' स्वामी जी-हमेशा रहने वाली स्थिति में रहने पर मन के गमनागमन से हर्ष- शोक नहीं होता। जिसका अनुभव स्वयं करते हो। अपने आप ! यदि मन के गमनागमन में हर्ष-शोक होता है तो तुमसे एक भी व्यवहारिक कार्य नहीं होंगे। रात-दिन तुम मन के निरोध करने में ही लगे रहोगे। सारी जिंदगी खत्म हो जायेगी। 'जी हाँ।' तो प्रश्न होता है कि हमेशा रहने वाली स्थिति में स्थिति के सिवाय क्या और कुछ अनुभव होता है? जी नहीं। हमेशा रहने वाली स्थिति में रहने पर उस स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव नहीं होता। क्या प्रमाण? 'मैं' था, 'मैं' हूँ, 'मैं' रहूँगा, अगर इसका अनुभव हो तो द्रष्टा, दर्शन, दृश्य का भी अनुभव हो। श्रोता, वक्ता का भी अनुभव हो, परन्तु हमेशा रहने वाली स्थिति में स्थित रहने पर स्थिति के सिवाय दूसरी स्थिति का अनुभव नहीं होता।
स्थिति के होते हुए स्थिति का अनुभव नहीं होता कि स्थिति है ही नहीं, इसलिए अनुभव नहीं होता? यदि स्थिति होय तब तो 'मैं' सर्व को जानता हूँ तो क्या स्थिति को न जानूँ?
मुक्तानुचर शास्त्री जी- 'जी।' स्वामी जी- ये श्रृंखला बंध रही है ना। मुक्तानुचर शास्त्री जी- जी हाँ। स्वामी जी- अगर उस स्थिति के सिवाय दूसरी भी स्थिति होय तब तो उसको भी 'मैं' जानूँ। जबकि 'मैं' सर्व को जानता हूँ तो उसको भी जानूँ हाँ! उस स्थिति के सिवाय और स्थिति का अनुभव नहीं होता। ये तो निर्विवाद सिद्धान्त है कि स्थिति दूसरी रहती ही नहीं सिवाय उस स्थिति के। तो फिर, दूसरी स्थिति को नहीं जानता, क्योंकि वो स्थिति नहीं है। जो हमेशा रहने वाली स्थिति है, उसमें रहकर दूसरी स्थिति का अनुभव नहीं होता या उससे विलग होकर दूसरी स्थिति का अनुभव नहीं होता। नहीं, उससे विलग नहीं होता, उसमें रहकर या वही होकर? नहीं, वही होकर। जो होकर 'मैं' स्थिति का, अस्थिति का अनुभव करता हूँ, उसको 'मैं' जानता हूँ। हाँ जी, 'मैं' जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कुछ नहीं जानता हूँ-बस, यही जानता हूँ, इसलिए उस स्थिति का अनुभव करो, जिसमें तुम हमेशा रहते हो। हूँ? याने मतलब ये है कि जिस मौन का अनुभव होता है या जिस मौन का अनुभव मैं करता हूँ, जिस मौन को 'मैं' जानता हूँ-वह इन्द्रियाँ अथवा मन का मौन है। क्योकि बोलना बंदकर दिया वाणी का मौन हो गया। देखना बंद कर दिया नेत्र का मौन हो गया। सुनना बंद कर दिया कर्ण इन्द्रिय का मौन हो गया। चलना-फिरना बंद कर दिया पैर का मौन हो गया। काम करना बंद कर दिया हाथ का मौन हो गया। मतलब ये है कि जिस इन्द्रिय का जो कार्य है वो इन्द्रिय जब अपने कार्य को छोड़ देती है उसको इन्द्रिय का मौन कहते हैं। इसी तरह मन जब अक्रिय हो जाता है, कोई न कोई साधन के द्वारा मन की दौड़-धूप जब बंद हो जाती है, संकल्प-विकल्प से रहित हो जाता है, निश्चय करने से बुद्धि रहित हो जाती है, चिंतन करने से चित्त रहित हो जाता है, तो जितनी इन्द्रियाँ हैं, जब अपने-अपने कार्य से संन्यास ले लेती हैं, कार्य का परित्याग कर देती हैं, चाहे किसी प्रकार से करें, यह सभी मौन हैं। जी हाँ। तो, इन्द्रियाँ जब तक कार्य करती रहती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण अथवा और कोर्ड भी इन्द्रिया जब तक के ये सब के सब कार्य करते रहते हैं, इनका जो अनुभव करता है, इनको जो जानता है, इनको जो देखता है और अपने-अपने कार्य को त्याग करके बैठ जाती हैं इन्द्रियाँ, उसको भी तो जानता है, अनुभव करता है, देखता है। तो, देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाले का नाम है 'महामौना' इसे महामौन कहते हैं। महामौन तो अपना स्वरूप ही है। बाकी इन्द्रियों का जो मौन है, उसे मौन कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस समय 'मैं' आत्मा किसी भी विषय का अनुभव करता हूँ, किसी भी देश, काल, वस्तु को देखता हूँ या जानता हूँ, उस समय मौन स्थिति में ही 'मैं' सर्व को जानता हूँ। मौन स्थिति में ही 'मैं' सर्व को देखता हूँ। मौन स्थिति में ही 'मैं' सर्व का अनुभव करता हूँ। क्योंकि 'मैं' स्वयं महामौन हूँ और इसलिए भी 'मैं' आत्मा महामौन हूँ कि मुझ आत्मा तक मन जा नहीं सकता, मौन हो जाता है। मुझ आत्मा का चिंतन चित्त कर नहीं सकता, मौन हो जाता है। मुझ आत्मा का बुद्धि निश्चय कर नहीं पाती, मौन हो जाती है। मुझ आत्मा को नेत्र इन्द्रिय देख नहीं सकती, मौन हो जाती है। मुझ आत्मा को वाणी कथन कर नहीं सकती, मौन हो जाती है। इसलिए कि 'मैं' आत्मा महामौन हूँ। किसी की शक्ति नहीं कि मुझ आत्मा तक पहुँचे और जो पहुँचेगा वो महामौन होकर ही पहुँचेगा। महामौन से जुदा होकर महामौन तक पहुँचना असंभव है। समुद्र से जुदा होकर नदी, समुद्र को नहीं जान सकती और समुद्र से मिलकर भी नदी समुद्र को नहीं जान सकती है। क्योकि जब समुद्र ही हो गई तब जानना-जनाना तो रहा ही नहीं। न जुदा होकर जान सकती है और न मिलकर जान सकती है। इसी तरह 'मैं' आत्मा को मुझ आत्मा से मन जुदा होकर नहीं जान सकता। (अंग्रेजी में - Mind can not knows, But he, Knows the mind.) अहा हा हा! मन जिसको नहीं जान सकता, मन को जो जानता है, तो मुझ आत्मा को मन नहीं जान सकता, मन को जो जानता है तो मुझ आत्मा को मन नहीं जान सकता। जुदा होकर नहीं जान सकता। चित्त जुदा होकर नहीं जान सकता, बुद्धि जुदा होकर नहीं जान सकती। वाणी जुदा होकर नहीं जान सकती। सबका 'राष्ट्रीयकरण' हो गया है। हाँऽऽ...। सबका राष्ट्रीयकरण हो गया है। इसको गणतन्त्र राज्य कहते हैं। प्रजातंत्र राज्य! प्रजातंत्र शासन का ये विधान है कि जो कुछ भी है (तुम्हारा घर-द्वार, तुम्हारा धन, जो कुछ भी तुम्हारे पास चल-अचल सम्पत्ति है) तुम्हारा कुछ नहीं, अरे, सभी कुछ राष्ट्र का है और हम तुम भी राष्ट्र के हैं। आज अगर शासन को जरूरत पड़े तो मकान से निकाल सकता है। यही समाजवाद शशासन तंत्र का विधान है। काम करो। छः घण्टे के बदले आठ घण्टे बाद और प्रजातंत्र हरी करो, व्यापारी हो व्यापार करो, नौकर हो तो आठ घण्टे डॉक्टर हा दस घंटे काम करो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा कुछ नहीं। सब राष्ट्र का है। अपना जरा भी न मानो। कमाओ डट के, मगर अपना मत मानो। राष्ट्र की रूपरेखा अभी पूरी तैयार नहीं बन रही है। चाहते तो सब यही है बुद्धिमान लोग कि भारत में प्रजातंत्र शासन स्थापित हो जाये, परन्तु हुआ नहीं। स्वामी जी? हाँ जी! तो क्या तुम भी देश के हो? और क्या आसमान के हैं हम। पैदा तो यहीं से हुए हैं हम- यहीं के हाड़-मांस से शरीर बना है और कहाँ के। और अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी गहर्नमेंट को तो? भैय्या, हम भी तैयार हैं, जाने को। तो तुम क्या करोगे? अगर गह्वर्नमेंट को जरूरत पड़ी तुमको फ्रंट पर भेजने के लिए मोर्चा पर, तो तुम क्या लड़ाई करोगे? अरे, जो यहाँ ललकार रहे हैं, वो वहाँ ललकारेंगे। वो बहादुर! योद्धाओं!! बढ़ो आगे !! जी हाँ...।
य एवं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥
(गीता 2/19)
अरे, आत्मा न मरती है, न मारती है किसी को यारों। अरे यारों बढ़ो आठो, मारो आतताइयों को। दुश्मनों को !! उसके अन्दर स्पिरीट (Sprit) भरेंगे। मोर्चे पर खड़े होकर अगर गह्वर्नमेंट को जरूरत पड़े, ले जाय, आज तैयार हैं, हम जाने को!!
महामौन की व्याख्या हो रही है। एक होता है मौन, एक होता है 'महामौन'। जो इन्द्रियों का मौन है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अथवा इन्द्रियाँ आदि उनका जो मौन, चतुष्ट-अन्तःकरण अथवा पंचकर्मेन्द्रियाँ, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ सभी जब अपने-अपने कार्य से संन्यास ले लेती हैं, उस मौन को इन्द्रियमौन कहते हैं और इन्द्रियों के करने को (इन्द्रियों की क्रियाओं को और अक्रिय हो जाने पर, उनके संन्यास ले लेने पर, उन सब बातों को जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है उसे 'महामौन' कहते हैं। ये महामौन 'मैं' आत्मा हूँ। इसलिए, महामौन कहलाता हूँ 'मैं' आत्मा। जिस आत्मा तक मन जाने में समर्थ नहीं होता, महामौन हो जाता है। चित्त समर्थ नहीं होता, अपनी चिंतन किया से संन्यास ले लेता है, महामौन हो जाता है। बुद्धि अपने निश्चय कार्य से संन्यास लेकर, मौन हो जाती है। वाह। वाणी, नेत्रादिक ये जितनी इन्द्रियाँ हैं, ये सब अपने-अपने कार्यों से संन्यास लेकर, मौन हो जाती हैं। इसलिए, 'मैं' आटमा को महामौन कहते हैं। दूसरी बीज यह है कि किसी भी विषय का 'मैं' आत्मा जब अनुभव करता हूँ, 'मैं' आत्मा चंचल होकर नहीं करता। (सत्संगी-चंचलता का भी अनुभव करता हूँ) स्वामी जी- हाँ! अरे, जिसका भी 'मैं' अनुभव करता हूँ, चंचलता का, स्थिरता का 'महामौन' ही होकर करता हूँ।
मुक्तानुचर शास्त्री जी - जी हाँ! स्वामी जी - और, ये सब मुझ आत्मा को जानना चाहें (महामौन को) तो उनको भी महामौन होना पड़ेगा। अरे, यार चोर को जानने के लिए चोर होना पड़ता है। चोर को जानने के लिए, जब चोर होना पड़ता है! चोर का पता लगाने के लिए -
कुनद हमजिंस हमजिंस परवाज ।
कबूतर वा कबूतर बाज व बाज ||
यारों, सजाति-सजाति से प्रेम होता है, सजाति-विजाति से नहीं। जो महामौन को जानने आता है, वो अपने आपको खोकर, अपने आपको मिटाकर, अपना वजूद खोकर ही मुझ आत्मा महमौन को जानेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए नदी का मिशाल दिया था कि नदी समुद्र से जुदा होकर न तो समुद्र को जानती है। अरे, जब जुदा ही हो गयी, अलग ही है, तब समुद्र क्या है, वो क्या जानेगी, और समुद्र होकर! तब भी नहीं जानती, किसी भी हालत में समुद्र को जानने में नदी समर्थ नहीं है। इसी तरह मुझ आत्मा से मन जुदा होकर, मुझ आत्मा को नहीं जान सकता। बुद्धि, चित्त, इन्द्रियाँ जुदा होकर जानना चाहें, विषय करना चाहें, तो नहीं कर सकतीं असमर्थ है।
गर जान जॉय - तब तो मुझ आत्मा की कोई 'पोजिशन' ही नहीं। और, जब 'मैं' ही हो जाता है तब ? तब भी नहीं जानेगी। जानना कहाँ है!
नाहं मन्ये सुवेदेति-नो न वेदेति वेव च ।
योनस्वद्वेव वद्वेव-नो न वेदेति वेव च ॥
इसलिए श्रुति कहती है-
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद 'सः ।
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम विजानताम् ॥
जो कहता है मैंने ब्रा को जाना, उसने नहीं जाना। जो कहता है नहीं जाना, उसने भी नहीं जाना। जो कहता है मैंने ब्रह्म को जाना है, उसने नहीं जाना, इसलिए कि जिस ब्रह्म को तू जानने का दावा करता है कि मैंने जाना। जाना, हा बहा तुझसे भिन्न है कि अभिन्न? अठार तुमने उस ब्रहा को मिल होकर जाना तो वो ब्रह्म ही नहीं है, तेरी बुद्धि तुझको धोखा दे रही है और अभिन्न करके जाना तो क्या जाना कुछ भी नहीं और अगर तू विकल्प करता है कि 'मैं' जानूंगा? तो किसको जानेगा। अगर तुमसे भिन्न है तो ब्रह्म नहीं और अभिन्न है तो जानेगा किसको?
इसलिए, जिज्ञासुओं उस स्थिति का अनुभव करो, जिस स्थिति में तुम हमेशा रहते हो। जानना-जनाना कुछ नहीं-ये भी एक बीमारी है, मुसीबत है। मुक्तानुचर शास्त्री जी- जी! स्वामी जी-किसको जानोगे? क्या चीज है जानने की? तब प्रश्न होता है कि जानना-जनाना नहीं है तो लोग कहते क्यों है कि- नो दाइ सेल्फ Know thyself ! नो दाइ सेल्फा अपने खुद को जानो, अपने खुद को पहिचानो। तुम कहोगे कि आपतो कहते हैं कि जानना ही नहीं है। 'आँया' क्या जानना? क्यों ऐसा कहा जाता है? अरे, कुछ नहीं जानना ही यही जानना है कि कुछ नहीं जानना है। बस। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो अपने 'मैं' को न जानता हो। 'मैं' हूँ इसको सब जानते हैं। एक छोटा-सा बच्चा भी। छोटे बच्चे से लेकर बुड्ढ़े तक, 'मैं' हूँ इसको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो, ये किसके लिए आता है कि खुद को जानो? खुद को पहिचानो? अरे, ये जानते हुए भी कहते हैं लोग कि 'मैं' नहीं जानता। और! भैय्या!! 'मैं' नहीं जानता। 'मैं' जानने को तो जानता हूँ। 'मैं' नहीं जानता, क्या नहीं जानता? 'मैं' की कोई सींग, पूँछ है-वो नहीं दिखाई देती हमको, उसको 'मैं' नहीं जानता। क्या चीज है, जिसको 'मैं' नहीं जानता? 'मैं' जानता तो हूँ-पर इसको नहीं जानता कि 'मैं' जानता हूँ। वाह!! शास्त्री जी- 'यही न जानना है।' स्वामी जी-अरे, यही न जानना है, यही जानना है। (हंसते हैं सभी) 'मैं' जानता हूँ, इसको नहीं जानता? ऐसा जो जानना है-यही जानना है। नहीं जमा का जी? शास्त्री जी- जी! जम गया !!
स्वामीजी- वाह! अब इसको ही जानने के लिए जिंदगी भर तुम शास्त्रों का अध्ययन करो, पढ़ो, लिखो, विचार करो आखिर में बस तुमको यही मिलेगा !! स्वामीजी। जब इतना ही मिलना है तो फिर ये पढ़ने-लिखने की क्या जरूरत है? 'शिवा' अरे, इतने दिन तक मत्था-पच्ची करोगे, तब तो इसकी कदर करोगे। मुक्तानुचर शास्त्री जी- 'जी!'
स्वामीजी- इतने दिन तक मत्थापच्ची करोगे, ठोकरें खाओगे तब न कदर करोगे इसकी। मगर भैय्या, पाओगे इतना ही। इससे आगे नहीं जाना है, इस। यही भगवान की महिमा है। इसलिए, 'मैं' आत्मा महामौन हूँ और हर हालत में 'महामौन' हूँ। देखो, जब 'मैं' किसी का अनुभव करता हूँ (अनुभव करो) किस स्थिति में अनुभव करता हूँ। तो, ये निश्चय हो गया और निश्चय हो गया होगा, तुम सब जिज्ञासुओं को कि जानना अनुभव करना मुझ आत्मा का ही धर्म है, मुझ आत्मा का ही काम है। मगर ये पता लगाओ कि एक सूत्र कल रात को लिखाया था ! उस स्थिति का अनुभव करो, जिसमें तुम हमेशा रहते हो। इसकी व्याख्या सुबह हुई थी। 'हाँ' -
1. उस स्थिति का अनुभव करो, जिसका अनुभव तुम हमेशा करते हो।
2. उस स्थिति को देखो, जिसको तुम हमेशा देखते हो।
3. उस स्थिति को जानो, जिसको तुम हमेशा जानते हो।
क्योकि भैय्या! अनुभव जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो इन्द्रियगम्य और एक अनुभवगम्य ? इन्द्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जाय, उसे इन्द्रियगम्य अनुभव कहते हैं। समझो... मन के संयोग से, बुद्धि के संयोग से, चित्त के संयोग से, प्राण के संयोग से अथवा और इन्द्रियों के संयोग से जो अनुभव किया जाता है, उसे इन्द्रियगम्य अनुभव कहते हैं और कहते भी है कि भाई ये अनुभवगम्य चीज है। जरा समझो इसको, शब्दों पर विचार करो। तो कहते हैं ये अनुभवगम्य चीज है-तो अनुभव तो हुआ 'मैं' और गम्य हुआ वो पदार्थ। जीऽऽ । अरे, इन्द्रियगम्य और अनुभवगम्या हाँ-अनुभव वो पदार्थ नहीं है अनुभवगम्य है। इन्द्रियगम्य और अनुभवगम्य, अब इन्द्रियगम्य किसको कहते हैं और अनुभवगम्य किसको कहते हैं? अरे, विकल्प तो इन्द्रियगम्य होता है और विकल्पाधार अनुभवगम्य बन गया ना!! अच्छा! तो सूत्र कहता है कि 'उस स्थिति का अनुभव करो, जिसका अनुभव तुम हमेशा करते हो।'
तो भैय्या। इन्द्रियों के द्वारा जिसका अनुभव होता है, उसको विकल कहते हैं। तो सर्वकाल में क्या विकल्प रहता है? नहीं रहता। और सूत्र कहता हाक उस स्थिति का अनुभव करो, जिसका अनुभव तुम हमेशा करते हो। तो विकल्प का अनुभव हमेशा होता ही नहीं? ना। मुक्तानुचर शास्त्री जी. जी। स्वामी जी-क्योकि विकल्प हमेशा रहता ही नहीं। विकल्प सर्वकाली। नहीं होता। तो अनुभव सर्वकालीन कैसे होगा? अच्छा, वाह!! देखो मस्ती में बैठे हो, आनन्द ले रहे हो इस समय। रोटी खा रहे हो, रास्ता चले जा रहे हो, पर 'मैं' आत्मा हूँ कि अनात्मा हूँ, सत्य हूँ कि असत्य हूँ, जड़ हूँ कि चेतन हूँ, द्रष्टा हूँ कि दृश्य हूँ, स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, इसका अनुभव नहीं हो रहा है। 'मैं' कौन हूँ, 'मैं' क्या हूँ, 'मैं' कैसा हूँ बिल्कुल नहीं। क्योकि ये सब विकल्प है, यह सभी इन्द्रियगम्य हैं। विकल्प का अनुभव हमेशा नहीं होता-विकल्याधार का...। अब डूब जाओ, इसी सागर में वाह! ये चीज है। इसके जानने के लिए महान् पुरुष कहते हैं 'नो दाई सेल्फ' Know thyself ! अपने आपको जानो, यही अपने आपको जानना है। वाह! शिव!! कैसी सहजावस्था, कैसी विलक्षण सहज समाधि है। शिव! उस स्थिति का अनुभव करो, जिस स्थिति का अनुभव तुम हमेशा करते हो। हमेशा भैय्या! विकल्पाधार का अनुभव करते हो-न कि विकल्प का। क्योंकि विकल्प सर्वकालीन नहीं होता। विकल्प कभी-कभी होता है, विकल्प क्या है-ये अमुक है, ये फलाँ चीज है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये धन है, ये मकान है- विकल्प कहते हैं इसको, सर्वकाल में नहीं रहता और सर्वकाल में न रहने वाला जो विकल्प है, इसका अनुभव इन्द्रियाँ करती हैं। ये इन्द्रियगम्य अनुभव कहलाता है। आँख विकल्प को देखती हैं, वाणी विकल्प का कथन करती हैं, मन विकल्प के लिए जाता है, चित्त विकल्प का चिंतन करता है, बुद्धि विकल्प का निश्चय करती है वाह! और क्या, जिस समय विकल्प पैदा होता है उसी समय ही इन्द्रियाँ पैदा होती हैं। उसके पहले इन्द्रियाँ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। विश्व के लिए चुनौती है, कोई आ करके सिद्ध करे। इन्द्रियाँ भी सर्वकाल में नहीं रहती, विकल्प को ही ग्रहण करने के लिए ही तुरंत इन्द्रियाँ तैयार होती हैं। देखने का विकल्प हुआ फट्ट से आँख आ गयी। सुनने का विकल्प हुआ कर्ण इन्द्रियाँ आ गयीं। हर समय इन्द्रियाँ नहीं रहती। हर समय तो यही...। बस, मस्त रहो। और इन्द्रियाँ बनाना नहीं पड़ता। अपने आप 'मैं' ही इन्द्रियाँ हो जाता हूँ। वाह!!
स्वामीजी-क्योंकि मेरे सिवाय तो कोई है ही नहीं। तो, इन्द्रियाँ कौन पैदा करेगा? सुनने की जरूरत पड़ती है तो, 'मैं' ही कर्ण इन्द्रियाँ बन जाता हैं। देखने की जरूरत पड़ती है, तब 'मैं' ही आँख बन जाता हूँ। सब कुछ • है' ही हो जाता हूँ। सब मेरी ही लीला है, मेरा ही खेल है। इसलिए, उस स्थिति का अनुभव करो, जिसमें तुम हमेशा रहते हो। क्या सुन्दर विलक्षण... पहले विकल्प पैदा होता है, उसके बाद उसको ग्रहण करने के लिए इन्द्रियाँ पैदा होती हैं इन्द्रियों को शास्त्र में 'गो' कहते हैं। इन्द्रियों के विषय को 'गोचर' कहते हैं। 'गो गोचर जहं लगि मन जाई।' गो माने इन्द्रिय। जैसे- तुमको गाय खरीद के लाना है, दूध पीना है, तो उस वक्त पहले गाय के खाने का इंतजाम करोगे। पंजाब में भूसा को तुड़ी कहते हैं। तुड़ी ले आओ, घास ले आओ खरीदकरा उसके रहने के लिए जगह का इंतजाम करो और जब सब इंतजाम हो जाता है, तब गाय खरीदकर लाते हो। इसी तरह इन्द्रियाँ हैं गऊ और उनका चारा है विषय और विषय है विकल्प रूप। तो पहले किसी विषय का विकल्प हो जाता है-ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये रूप • है, ये रस है, ये गंध है। किसी विषय का पहले विकल्प होता है-उसको ब्रहण करने के लिए गाय रूप इन्द्रियाँ आ जाती है और वो भी इसलिए कहा जा रहा है कि-जब तुम विषय मानते हो। अगर तुम्हारी दृष्टि में विषय और इन्द्रियाँ हैं तो इस प्रकार और नहीं तो सर्वकालीन स्थिति तो है ही। 'उस स्थिति का अनुभव करो, जिसमें तुम हमेशा रहते हो।' उस स्थिति का अनुभव करो, जिसका तुम हमेशा अनुभव करते हो। 'मैं' आत्मा इन्द्रियगम्य का अनुभव करता हूँ कि अनुभवगम्य का अनुभव करता हूँ? अब ये दूसरी कोटि है। अनुभवाम्य का अनुभव करता हूँ। अनुभवगम्य-अहंगम्या अरे, भाई। विकल्प जब नहीं रहा तो विकल्प जिस पर आधारित है। अच्छा, जो अनुभवगम्य है वह इन्द्रियगम्य नहीं, तो जो अनुभवगम्य है वह 'मैं' ही तो हूँ। अनुभवगम्य क्या है, अनुभवगम्य कैसा है, अनुभवगम्य कौन है? इसको 'मैं' बताऊँ तो कैसे बताऊँ? अगर 'मैं' बताता हूँ तो अनुभवगम्य नहीं, वाणीगम्य हो जाता है, मुक्तानुचर शास्त्री जी-वूनों कोती ले करलई हे जी। स्वामी जी हाँ, नहीं गा दूनो कोती ले करलई हे जी, मुक्तानुचर शास्त्री जी- सब गड़बड़-सड़बड़ मामला है। हाँ, अगर कुछ कहता हूँ तो वाणीगम्य, वाणी का विषय हो गया और नहीं कहता... शास्त्री जी- तो कौन बैठेगा यहाँ। स्वामीजी-इसलिए, जो अनुभवगम्य है वह 'मैं' ही हूँ। दूसरी चीज है ही नहीं अनुभवगम्य, सिवाय मुझ आत्मा के! बाकी सब इन्द्रियगम्य है और अनुभवगम्य है वही हमेशा रहने वाली स्थिति है। क्योंकि, जितने लोग अभी बैठे हो अगर बुद्धि से सोचो, बुद्धि से विचार करो, बुद्धि से निश्चय करो! जो हमेशा रहने वाली स्थिति है... अगर बुद्धि विचार करें कि कैसी स्थिति है यह? मुक्तानुचर शास्त्रीजी- बुद्धीच नई रहे। स्वामी जी-हाँ, बुद्धि खो जाती है। मन अमन हो जाता है, चित्त-चित् हो जाता है। अरे भैय्या! जिसने चोर को छुवा, चोर हो गया। छुवा-छुई का खेल देखे हो कभी, एक लड़का चोर बनता है-तो चोर लड़का जब दूसरे को छूता है, जो छूता है (चोर लड़का) उसका चोरपना गायब हो जाता है। जो छुवाता है वह चोर बन जाता है। कह गए दास कबीरा तो जिसने भगवान आत्मा 'मैं' को छुवा? गायब। वाह! तो उस स्थिति का अनुभव करो जिसका अनुभव तुम हमेशा करते हो। वाह! मस्ती में बैठे हो, रोटी खा रहे हो, रोटी बना रहे हो, रास्ता चले जा रहे हो। पर पता भी तो लगे कि 'मैं' कौन हूँ। वाह! क्या सुन्दर स्थिति है। यही महामौन पद है। 'महामौन'। सत्संगी - जिसके स्मरण मात्र से सारा विश्व मौन हो जाता है। स्वामीजी हाँ, वही महामौन। जिस महामौन के स्मरण मात्र से सारा विश्व महामौन हो जाता है। मन ही तो विश्व है। मन मौन हुआ कि सारा विश्व मौन हुआ। शास्त्री जी- जी हाँ। शास्त्री जी-
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ।।
गीता 10/38
सारा विश्व मौन हो जाता है। उस स्थिति का अनुभव करो, जिसका तुम हमेशा अनुभव करते हो। तो, यहाँ पर प्रश्न होता है कि हमेशा रहने वाली स्थिति तो रहती ही है , क्या वह अनुभव की चीज है? तो क्या देखने की चीज है। अनुभव की चीज है।
सब मिलकर स्वामीजी के साथ ग़ज़ल गाते हैं।
उफ़ है ऐसी जिंदगी जिसकी मिला साकी नहीं । हाँ।
शर्म को भी शर्म है 'वाह' पीना कभी बाकी नहीं । हाँ।।
वो नशा क्या जिसको तुरसी एकदम देवे उतार।
एक मर्त्तबे चढ़के उतरना फिर कभी बाकी नहीं।
सूरतें लाखों हैं पर सूरतगरी है एक की।
देखते ही जीना मरना फिर कभी बाकी नहीं ।
होश को बेहोश करती लानते देते हैं लोग ।
मगर यहाँ ॥.....
बेहोश भी बेहोश है होश आना बाकी नहीं ।
साकिया ने क्या पिलाया कब पिलाया वाह-वाह ।
अरे, मैं कहाँ और तू कहाँ दुनियाँ कहाँ बाकी नहीं ।
जो मय है एक सौ पैमाना ए दिल में भरी,
'मुक्त' पीता व पिलाता बाकी भी बाकी नहीं । हाँ
उम्र है ऐसी जिंदगी जिसको मिला साकी नहीं । हाँ।।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
विविध
■गर हकीकत में आशिक हो, तो निर्विकल्प किले के भीतर सहजानन्दी शाही तख्त पर माशूक बैठा है, नकाबे आसमान चीरकर अंदर घुस जाओ।
■ आशिक माशूक जिस वक्त दोनों मिलते हैं, उस वक्त दोनों की हस्ती खत्म हो जाती है। महज इश्क रह जाता है।
■ नजरे माशूक आशिके वतन खत्म कर देती है।
कीर्ति, महारानी माया के सिर का मुकुट है। कंचन, कामिनी अनन्त श्री विभूषित महारानी माया के दोनों कानों के कुण्डल हैं। वासना परिधान है। देहाभिमान खड्ङ्ग है। अज्ञानी जीव वाहन है। कामादिक विकार सेना है। त्यागाभिमानी बलिपशु है। मान्यता जगत् साम्राज्य है। ऐसी स्वनामधन्या, महामहिमामयी, विश्वसुन्दरी, स्वमुख विमोहिनी, दयाहीन हृदयवाली, विश्व को तिरछे नयनों से देखने वाली, श्रीमती साम्राज्ञी महामाया महारानी का पति महाराजाधिराज समस्त चराचर का सम्राट सर्व का अस्तित्व एवं सर्व का 'मैं' अपना आप भगवान आत्मा 'मैं' है।
आशिके माशूक हूँ, इक तरफा मजा है।
दीवाना हूँ मैं जिसका, वह दीवाना है मेरा ।।
■ यार का मिलना इतना आसान है, जिसकी आसानी ही परेशानी है।
■ यार इतना खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती ही बदसूरती है।
■ यार इतना लबालब है, जिसमें तमाम खामियाँ ही नजर आती हैं।
■ दिल का दरवाजा खटखटा कर आजादी आवाज दे रही है कि ऐ नादान! जिसकी तुझको तलाश है, वह तेरे चारों तरफ है, जिसे कहते हैं आजादी। खातिर कर, प्यार कर, दीदार कर, बेहोश हो, खामोश हो, फरामोश हो।
कहूँ क्या मैं तुम कौन हो और क्या हो ।
हो सबसे मिले और सबसे जुदा हो ||1||
प्रकृति भी तुम्ही पुरुष भी तुम्हीं हो ।
कहीं तुम पुजारी कहीं देवता हो ||2||
तुम्हारा ही है खेल यह विश्व सारा ।
तुम्हीं अग्नि पृथ्वी गगन जल हवा हो ||३||
नहीं में नहीं हो तो हाँ में हाँ तुम ।
तुम्हीं नेस्त और अस्ति की व्याख्या हो ||4||
निलज्जे हो इतने कि हो सर्व व्यापक ।
लजीले हो इतने अगोचर सदा हो ||5||
□ आज्ञा की अवहेलना प्रमाद का स्वागत (सन्मान) है।
□ व्यक्तित्व के अहं भाव में अवहेलना निहित है।
□ मन के ग्रहण में व्यक्तित्व का अस्तित्व है।
□ मन का ग्रहण क्षुद्रता (दुर्बलता, नीचता) का प्रतीक है।
□ वैकल्पिक व्यक्तित्व में क्षुद्रता की रेखा है।
□ स्वार्थी हृदय को किसी भी क्षेत्र में सेवा का अधिकार नहीं।
□ श्री खण्ड की छत्रछाया में बैठकर विष्टी में स्नान करना कोई बुद्धिमानी नहीं है।
आत्मनिष्ठा अंतरिक्ष यान है। निर्विकल्पता अंतरिक्ष है। सहजपद अन्तरिक्ष पद है। सहजानन्दी यात्री है। अनुभूति कैमरा है। अनिर्वाच्यता टेलीविजन है। जहाँ पर 'मैं' के अतिरिक्त कुछ भी नहीं यही वहाँ का चित्र है। अन, वाणी रूप पृथ्वी से परे कल्पनातीत पद यही अनन्त योजन दूरी है।
□ स्वरूप की विस्मृति ही माया है।
□ अरे, ही स्वरूप विस्मृति है।
□ अरे, का अत्यान्ताभाव ही आत्मा का सतत् चिंतन है। निर्विकल्पता का विकल्प ही निर्विकल्पता का बाधक है।
□ आत्म चिंतन का संकल्प ही आत्म चिंतन में विक्षेप है।
□अरे का अत्यन्ताभाव ही सतत् आत्म चिंतन है। इसका भाव यह है कि जब आत्मा 'मैं' से भिन्न कुछ है नहीं तो आत्मा का चिंतन इसके सिवाय और क्या हो सकता है अथवा यूँ कहो कि कुछ भी चिंतन न करना, यही आत्म-चिंतन है। 'मैं' के अतिरिक्त कुछ भी न देखना, यही आत्मदर्शन है। 'मैं' के अतिरिक्त कुछ भी न जानना यही आत्मज्ञान है। बस, इसी सम्राट पद पर निरन्तर स्थित रहो।
□ संत द्वारा सन्मान प्रमाद का प्रतीक है।
□संत की झिड़कियाँ क्षुद्राभिमान का काल है।
□ संत हृदय संत की फटकार का भिखारी होता है। क्षुद्र हृदय सम्मान का।
□व्यक्तित्व का अनादर संतों के सम्मान का हाजमा चूर्ण है।
□ व्यक्तित्व का अनादर संत शरणागति का फल है।
□ संत शरणागति भगवान की शरणागति का पर्याय है।
□ मन की तृष्णा रूपी क्षुधाग्नि को शांत करने के लिए कुछ भी चिंतन न करना ऐसा ब्रह्म चिंतन ही ब्रह्मचर्य है।
□ विश्व रूपी गृह में स्थित होने वाला ही गृहस्थ है।
□ वासना रूपी बनिता से दूर सहजावस्था रूपी तप में आरुढ़ होना ही वानप्रस्थ है।
□ त्याग माने त्याग, ग्रहण माने ग्रहण, दोनों विकल्पों का संन्यास ही संन्यास है।
□चारों आश्रमों के भाव के अभाव पद में जो स्थित सोई अवधूत है।
□ अंतरिक्ष यात्री बनो।
□ जो अंतरिक्ष में रहता है, वही अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है।
|| माया पंचकम् ॥
निरुपम नित्य-निरंशकेऽप्यखण्डे मयिचिति सर्व-विकल्पाविशुन्ये ।
घटयति जगदीश-जीवभेदं त्वघटित-घटना-पटीयसी माया ||1||
श्रुति-शत्-निगमान्त-शोधकानप्यहरु धनादि-निदर्शनेन सद्यः ।
कलुषयति चतुष्पदाद्यभिन्नान् त्वघटित-घटना-पटीयसी माया ||2||
सुखचिदखण्ड विवोधमद्द्वितीयं वियदनलादि-विनिर्मिते नियोज्य ।
भ्रमयति भवसागरे नितान्टतं त्वघटित-घटना-पटीयसी माया ||३||
अपगत-गुण-वर्ण-जाति-भेदे सुख-चित-विप्र-विडाद्यहंकृति च ।
स्फुटयति सुत-वार-गेह-मोहं त्वघटित-घटना-पटीयसी माया ||4||
विधि हरिहर-भेदमप्यं खण्डेवत विरचय्य बुधानपि प्रकामम् ।
भ्रमयति हरिहर-विभेद-भावान् व्वघटित-घटना-पटीयसी माया ||5||
- आद्यजगद्गुरु शंकराचार्य
कहीं होय विरंचि सृष्टि रचता अनेक भाँति ।
कहीं होय मुकुन्द सृष्टि पालत अपेला है ।
कहीं होय महेश भेष सृष्टि खास नाश करे ।
या प्रकार तीन रूप धारे तीन बेला है ।
कहीं जै गोविंद देव वृन्द होय आनन्द करे ।
कहीं बनि दैत्य-देव झगर झमेला है ।।
कहाँ लोँ बखानिये न जानिये सो वाकि गति ।
है सही अकेला पर अनेक खेल-खेला है।
मुक्ताष्टक
यस्मानुभूति विशदी कृत शास्त्र वस्त्राम् ।
शृंगार षोडशरतामिव तत्वनिष्ठाम् ॥
श्रद्धामयस्य पुरुषस्य पपात तेजो ।
हट्वा तपस्टवजनि लोक हिताय मुक्तः ||1||
अहो अलं श्लाघ्य तमं कृतं कुलम् ।
अहो अलं कश्यप गोत्र वृत्तम् ।।
अलंकृता सा जननी गत व्यथा ।
निरीक्षती सुस्मित सुन्दरमुखम् ||2||
सत्याशिषोहि गुरवः कुल देवता च ।
नान्दी मुखेन पितरः स्वयमेव तृप्ताः ॥
आनन्दमय कृत पूर्व निपात सिद्धो ।
जातः पिता सुत मुखाम्बुज दर्शनेन ||3||
लोकाभिरामं सकलाभिरामम् ।
झण्डापुरन्धी नयनाभिरामम् ।
दृष्ट्वा गृहीनां गृहिणी जनानाम् ।
हढ़ा प्रवृत्तिः प्रति पुत्रभावम् ||4||
स्वयोगमाया रुचिराङ्ग विग्रहः ।
क्रीडा करिष्यन्निव सर्वविग्रहान् ।।
सनित्यमुक्तो विदुरेति नामकः ।
वात्सल्यतायां परतंत्रवद्धृतः ।।5।।
त्रिशूल चक्राङ्कित चारू पावयोः ।
संलग्नधूलि प्रतिलब्ध कामौ ।।
वचाङ्गुली याविव देव देवौ ।
यत्रैव तत्रैव हि सर्वदेवाः ||6||
ययेव तीर्थीकृत जन्म भूमिः ।
स एवतीर्थी कृत सर्व भूमिः ।
यः सेवकानां हृदयं पुनाति ।
स एवस्यान्मद् वचसो विभूतिः ॥7॥
हे ज्ञान मान वसुवर्धन दृष्टिमात्रात् ।
स्वात्मप्रदोऽस यदहं तदहं त्वमेव ।।
शय्यासनाटन विकत्थन भोजनादि ।
ष्वैक्यात्तथापि यदधं तदधं क्षमस्व ||8||
मुक्ताष्टकमिदं पुण्यम् सन्तरूप हरेस्मरन् ।
पठन्नसृण्वन्नरोति । सर्वं सिद्धिन्नसंशयः ||9||