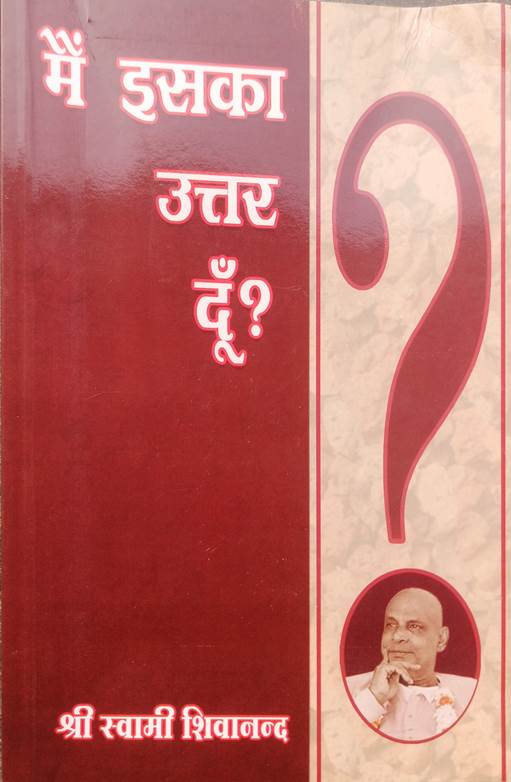
मैं इसका उत्तर दूँ?
MAY I ANSWER THAT?
का अविकल अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती
अनुवादिका
श्री स्वामी शिवाश्रितानन्द माता जी
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण : २०२०
(१,००० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
ISBN 81-7052-259-5
HS 20
PRICE: 130/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा
प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी प्रेस,
पत्रालय : शिवानन्दनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड,
पिन : २४९१९२' में मुद्रित।
For online orders and Catalogue visit: dlsbooks.org
प्रकाशकीय
यह पुस्तक परम पावन गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज की विभिन्न प्रकाशित रचनाओं में से संकलित की गयी है, जिसमें उनकी तीस के दशक के अन्तिम भाग की कतिपय प्रारम्भिक कृतियाँ भी सम्मिलित की गयी हैं।
पुस्तक में लिये गये प्रश्नों एवं उत्तरों की शृंखला में कुछ अत्यधिक सामान्य प्रतीत होने पर भी, आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करने वाले जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली शंकाओं का अत्यन्त सशक्त समाधान प्रस्तुत करने वाले हैं। इन उत्तरों एवं स्पष्टीकरणों को जो अनमोल प्रतिष्ठा प्रदान करता है, वह इसकी प्रामाणिकता का होना है, जो केवल एक सन्त के अन्तर्बोध ही नहीं, अपितु निजी अनुभव की भी उपज हैं।
स्वामी शिवानन्द ऐसे सन्त थे जिनकी सर्वप्रथम रुचि, अपितु हम तो कहेंगे, सर्वप्रथम प्रेम था आध्यात्मिक साधकों से, योग-विद्यार्थियों से। शिवानन्द जी का जीवन ही उनकी सेवा हेतु था, और यह अनमोल ग्रन्थ उन महान् गुरुदेव के सेवा भाव का ही परिणाम है।
हम आशा करते हैं कि साधक जगत् प्रत्येक पृष्ठ के ध्यानपूर्वक पठन के साथ यथेष्ठ रूप से लाभान्वित होगा और साधक-जन अपनी आध्यात्मिक परिपूर्णता के संघर्ष में असाधारण मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्राप्त करेंगे।
सद्गुरुदेव के दिव्य आशीर्वाद सभी पर हों!
शिवानन्दनगर -द डिवाइन लाइफ सोसायटी
१
हमें भगवान् में विश्वास क्यों करना चाहिए?
क्योंकि भगवान् प्रत्येक मानव के लिए नितान्त आवश्यक हैं। यह सबके लिए एक अनिवार्य अथवा परम आवश्यकता हैं। अविद्या या अज्ञान के कारण दुःख सुख की तरह प्रतीत होता है। वास्तव में तो यह संसार दुःखों, कष्टों, कठिनाइयों और मुसीबतों से भरा हुआ है। संसार एक आग का गोला है। राग, द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या से भरा हुआ अन्तःकरण जलती हुई भट्ठी के समान है। हमने स्वयं को जन्म, मरण, वृद्धावस्था, रोग और दुःख से छुटकारा दिलाना है। यह केवल भगवान् में विश्वास करने से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। धन-सम्पत्ति और पद या शक्ति हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकते। चाहे हमें सारे संसार का अधिराज्य प्राप्त हो जाये, तो भी हम चिन्ता, तनाव, भय, निराशा इत्यादि से मुक्त नहीं हो सकते। यह तो केवल भगवान् में विश्वास करने तथा उसके परिणाम स्वरूप ध्यान के द्वारा भगवद्-साक्षात्कार करने से ही हमें सच्ची और सदा रहने वाली प्रसन्नता मिल सकती है और हम सब प्रकार के भय एवं चिन्ता से तथा हर क्षण की यातना से छूट सकते हैं। भगवान् में विश्वास हमें हर समय उनका स्मरण करने को प्रेरित करेगा, उनका ध्यान करने की प्रेरणा देगा और इसी के माध्यम से हम भगवद्-साक्षात्कार की ओर अग्रसर होंगे।
२
ईश्वर के अस्तित्व को न मानने से क्या हानि है?
यदि हम ईश्वर के होने में विश्वास नहीं करते, तो हमें इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से कष्ट सहने पड़ेंगे। अज्ञानी अविश्वासी संशयात्मा विनाश को प्राप्त होते हैं। उन्हें जरा से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संशयात्मा के लिए न तो इस संसार में सुख है न ही इससे परे दूसरे लोकों में है। जिन्हें भगवान् में विश्वास नहीं है, उन्हें यह ज्ञान ही नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत। उनकी विवेक-शक्ति नष्ट हो चुकी है। वे असत्यवादी, अभिमानी एवं अहंकारी हैं। वे अत्यधिक लोभी, क्रोधी और कामी हो जाते हैं। वे अनुचित साधनों से धन अर्जित करते हैं। उनकी वृत्ति राक्षसी हो जाती है। वे अनेकों प्रकार के घिनौने अपराध करते हैं। उनके जीवन के कोई आदर्श नहीं होते। वे आसुरी योनियों में गिरा दिये जाते हैं। वे जन्म-जन्मान्तरों तक निम्न से निम्नतम योनियों में भटकते रहते हैं।
लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले, दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली जिले के करूर के निकट नेरूर नगर में सदाशिव ब्रह्येन्द्र नाम के एक सुप्रसिद्ध योगी-ज्ञानी रहते थे। वह 'ब्रह्मसूत्रवृत्ति' तथा 'आत्मविद्याविलास' एवं बहुत से अन्य ग्रन्थों के रचयिता हैं। एक बार जब वे कावेरी नदी के तट पर समाधि में लीन थे तो बाढ़ आ गयी और उन्हें बहा कर कहीं और ही फेंक गयी। वे बहुत गहरे रेत के ढेर में दब गये। मजदूर खेत में हल चलाने के लिए चले गये। उनके हल की चोट योगी के शिर में लगी और रक्त बह निकला। उन्होंने खुदाई की और यह देख आश्चर्यचकित रह गये कि एक योगी समाधिस्थ बैठे हुए हैं।
एक अन्य समय पर सदाशिव ब्रह्मेन्द्र अवधूत-वेश में मुसलिमों के एक सरदार के जनानखाने में नग्नावस्था में प्रविष्ट हो गये। सरदार उन सन्त पर अत्यधिक क्रोधित हो उठा। क्रोध में आग-बबूला हो कर उसने महात्मा की एक भुजा काट डाली। सदाशिव ब्रह्मेन्द्र एक शब्द भी बोले बिना तथा कष्ट का कोई भी भाव चेहरे पर लाये बिना चुपचाप चल दिये। सन्त की अद्भुत स्थिति देख कर सरदार आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ गया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से कोई महात्मा, कोई महामानव है। उसे अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ और वह सन्त से क्षमा माँगने के लिए उसके पीछे-पीछे चल पड़ा। सदाशिव को पता ही नहीं चला था कि उसकी भुजा काट दी गयी है। जब सरदार ने शिविर में घटने वाला सारा वृत्तान्त सुनाया तो सदाशिव ने उसे क्षमा करते हुए अत्यन्त सहज भाव से अपनी कटी हुई भुजा वाले कन्धे को स्पर्श किया। सदाशिव ब्रह्मेन्द्र के छूते ही वहाँ नयी भुजा आ चुकी थी। इस सन्त के जीवन ने मेरे मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। मैं इस निश्चित परिणाम पर पहुँच गया कि इन वस्तु-पदार्थों से अलग, इस मन और इन्द्रियों से परे एक स्वतन्त्र एवं उदात्त दिव्य जीवन है। सन्त इस संसार से पूर्णतया अनभिज्ञ था। उनकी भुजा जब काटी गयी, तब उन्हें किंचित् भी ज्ञात नहीं हुआ। वह उस समय दिव्य चेतना में लीन रहे होंगे, वह उस समय परम तत्त्व से एक होंगे। सामान्य लोग सुई की चुभन से कराह उठते हैं। जब मैंने आप्त व्यक्तियों से सन्त सदाशिव के जीवन का यह अद्भुत वृत्तान्त सुना और जब पुस्तक में पढ़ा तो मेरी यह धारणा अत्यन्त दृढ़ हो गयी कि एक दिव्य सत्ता है और एक ऐसा शाश्वत जीवन है जहाँ समस्त दुःख समाप्त हो जाते हैं, जहाँ सभी इच्छाएँ सन्तृप्त हो जाती 35/6 और व्यक्ति परम आनन्द, परम शान्ति तथा परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
३
ब्राह्ममुहूर्त का अर्थ क्या है ? हमारे ऋषियों ने इसकी इतनी प्रशंसा क्यों की है?
प्रातः ४ बजे के समय को ब्राह्ममुहूर्त कहते हैं। क्योंकि भगवान् या ब्रह्म पर ध्यान करने के लिए यह समय अनुकूल है, इसलिए इसे ब्राह्ममुहूर्त कहा गया है। इस समय मन विशेष रूप से अत्यन्त शान्त एवं अविक्षुब्ध अथवा निर्मल होता है। यह सांसारिक विचारों, चिन्ताओं और तनावों से मुक्त होता है। इस समय हमारा मन कोरी चादर अथवा कोरे कागज की तरह होता है और अभी लौकिक संस्कारों से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। सांसारिक विकर्षणों के प्रवेश होने से पहले मन को सरलता से मोड़ कर अनुकूल साँचे में ढाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस समय वातावरण में अधिक सत्त्वगुण की प्रधानता होती है। बाह्य जगत् की चहल-पहल और शोरगुल ने अभी वातावरण को प्रभावित नहीं किया होता।
४
हिमालय के गुरुओं के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं?
समस्त गुरुओं का एक गुरु है, जो आपके हृदय में निवास करता है। अपनी दृष्टि को अन्तर्मुखी करें, इन्द्रियों को बाह्य वस्तु-पदार्थों की ओर जाने से रोकें और अपने अन्तर्वासी की सहायता माँगें। उसी में स्थिर हो जायें। स्वयं की उनके साथ पहचान बनायें। हिमालय के इन गुरुओं के सम्बन्ध में पुनः मुझसे चर्चा न करें। आप भ्रमित हो जायेंगे।
५
जप और ध्यान में क्या अन्तर है?
भगवान् के नाम को मौन रहते हुए निरन्तर दोहराने को जप कहते हैं। भगवान् के एक ही विचार के सतत प्रवाह का नाम ध्यान है। जब आप 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्र को दोहराते जाते हैं, तो यह विष्णु-मन्त्र का जप कहलाता है। जब आप विष्णु भगवान् का हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण किये हुए स्वरूप का चिन्तन करते हैं, उनके कानों में कुण्डल, शीश पर मुकुट, रेशमी पीताम्बर इत्यादि धारण किये हुए का चिन्तन करते हैं तो यह ध्यान है। जब आप भगवान् के गुणों, जैसे सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता इत्यादि का चिन्तन करते हैं तो यह भी ध्यान है।
६
भगवान् की कृपा से मेरे लिए सब कुछ हो जायेगा, फिर मुझे साधना करने की क्या आवश्यकता है ?
यह धारणा गलत है। भगवान् उनकी सहायता करते हैं, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। भगवान् की कृपा-वृष्टि केवल उन पर ही होगी जो परिश्रम करते हैं। भगवान् की कृपा की वर्षा व्यक्ति के समर्पण के अनुपात में होती है। जितना अधिक आपका समर्पण होगा, उतनी ही अधिक उनकी कृपा आप पर होगी, भगवान् आपके लिए आत्म-समर्पण करेंगे, आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते। उठें और परिश्रम में जुट जायें। संघर्ष करें! लगे रहें! दृढ़ रहें! भगवान् आप पर अपनी कृपा की वर्षा करेंगे।
मीरा ने सब-कुछ त्याग दिया था। उसने राज्य, पति, सगे-सम्बन्धी, मित्र-सखा और धन-दौलत-सबका परित्याग कर दिया था। वह दिन-रात अपने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करती रहती थी। उसने प्रेमाश्रु बहाये। उसने खाना-पीना छोड़ दिया। उसकी देह सूख कर काँटा हो गयी। किन्तु उसका मन सदा भगवान् कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था। केवल तभी भगवान् ने उस पर अपनी कृपा की वर्षा की।
७
क्या आप मुझे आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई अत्यन्त सरल किन्तु ठोस प्रमाण दे सकते हैं?
आप आये दिन 'मेरा शरीर', 'मेरे प्राण', 'मेरा मन', 'मेरी इन्द्रियाँ' कहते हैं। यह स्पष्ट बताता है कि आत्मा शरीर, मन, प्राण और इन्द्रियों से पूर्णतया भिन्न है। यह मन और शरीर आपके सेवक अथवा उपकरण हैं। यह आपसे उतने ही अलग हैं जितना कि यह तौलिये, कुर्सियाँ और प्याले इत्यादि हैं। आप अपने शरीर को इसी तरह से धारण किये हुए हैं, जैसे कि हाथ में यह छड़ी। आप अपने इस शरीर के मालिक हैं। यह शरीर आपकी सम्पत्ति है। यह देह, मन, इन्द्रियाँ इत्यादि आत्मा नहीं हैं, किन्तु उससे सम्बन्धित हैं।
८
यदि भगवान् इन्द्रियों की पहुँच से परे है, तो वह एक अस्तित्वहीन, एक शून्य मात्र, एक नकारात्मक धारणा और एक दुर्बोध कल्पना ही होनी चाहिए। इन्द्रियों की पहुँच से परे ? यह कैसे हो सकता है? मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं कर सकता। मैं वैज्ञानिक हूँ। मुझे सही-सही लेबोरेटरी प्रमाण चाहिए।
आप लेबोरेटरी के प्रमाण चाहते हैं? बहुत बढ़िया ! आप उस असीम सर्वव्यापक परमात्मा को अपनी परखनली, धौंकनी और रासायनिकों में सीमित करना चाहते हैं! भगवान् आपके रसायनों का उद्गम हैं। वह आपके एटम, इलेक्ट्रोन और मॉलिक्यूल-सभी का आधार हैं। उनके बिना कोई एटम या इलेक्ट्रोन हिल भी नहीं सकेगा। वह अन्तर्यामी हैं। वह नियन्ता हैं। उनके बिना अग्नि जल नहीं सकती, सूर्य चमक नहीं सकता, वायु चल नहीं सकती। उनके बिना आप देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते। वह सभी वैज्ञानिक सिद्धान्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त, संसक्ति (कोहिजन) का सिद्धान्त, आकर्षण और विकर्षण का सिद्धान्त इत्यादि सभी सिद्धान्तों को प्रदान करने वाले हैं। उनके आगे श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक हों। उनकी कृपा से आपको समस्त विज्ञानों के विज्ञान, ब्रह्मविद्या का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जायेगा तथा मोक्ष-प्राप्ति हो जायेगी।
९
आजकल साधक ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त करने में असफल क्यों रह जाते हैं?
विकास की किसी भी एक स्थिति-विशेष पर पहुँचते ही वह अपनी शक्तियों को प्रवचन देने में, शिष्य बनाने में, पुस्तकें छपवाने में गँवाने लग जाते हैं। वह नाम-यश के दास बन जाते हैं। यही कारण है कि वह जीवन के परम लक्ष्य-ईश्वर-साक्षात्कार को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
१०
कुण्डलिनी कैसे जागृत की जा सकती है? क्या केवल जप के द्वारा इसे जागृत किया जा सकता है?
आसन, प्राणायाम, मुद्राओं और जप के अभ्यास से तथा गुरु की कृपा से कुण्डलिनी जागृत की जा सकती है। मेरी पुस्तक 'कुण्डलिनीयोग' देखें।
हाँ, अकेला जप इसे जागृत करने के लिए पर्याप्त है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। श्री समर्थ रामदास जी ने नासिक के निकट, ताकलि गाँव में, गोदावरी नदी में खड़े हो कर 'ॐ श्री राम जय राम, जय जय राम' मन्त्र का तीस करोड़ बार जप करके कुण्डलिनी जागृत कर ली थी।
११
मन के तीन दोष क्या है? कृपया मुझे ठोस एवं निश्चित उदाहरण दीजिए।
यह हैं काम, क्रोध और लोभ इत्यादि मन की मलिनताएँ तथा विक्षेप, अर्थात् मन की चंचलता एवं आवरण, अर्थात् अज्ञान का परदा।
एक कीचड़ से भरी हुई झील है और उसके ऊपर काई जमी हुई है। प्रचण्ड वायु तीव्र वेग से चल रही है। अब, यह झील मन है। कीचड़ से भरे होना मल का द्योतक है। वायु के वेग से जल में होने वाली हलचल प्राणों की गति से होने वाले मन के विक्षेप को सूचित करती है। पानी के ऊपर जमी हुई काई अज्ञान के आवरण को दर्शाती है।
१२
मन को सूक्ष्म और पवित्र कैसे किया जा सकता है ?
जप करें। निष्काम सेवा करें। मन की गहराई से भगवान् से प्रार्थना करें। सत्संग करें। ध्यान करें। गीता और उपनिषदों का स्वाध्याय करें। अकेले रहें। छह महीनों के लिए सात्त्विक भोजन करें। मांस, मछली, अण्डे, मद्यपान, मिर्च, तेल, चीनी, प्याज और लहसुन का परित्याग कर दें।
१३
भक्ति और ज्ञान में क्या अन्तर है?
भक्ति समर्पण है। ज्ञान की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उसका साधन भक्ति है। भावना-प्रधान स्वभाव वाले लोगों के लिए यह उपयुक्त मार्ग है। इसमें आत्म-समर्पण अथवा आत्म-निवेदन की आवश्यकता है। यह मार्जारीयोग है। बिल्ली का बच्चा जोर से रोता है और उसकी माँ तुरन्त दौड़ कर आती है तथा बिलौटे को मुख में पकड़ कर उठा लेती है। इसी प्रकार भक्त द्रौपदी और गजेन्द्र की तरह जोर से रोता है तथा भगवान् कृष्ण तुरन्त उसकी रक्षा के लिए एवं कृपा-वृष्टि करने के लिए दौड़े आते हैं। भक्ति-मार्ग में केवल सच्ची गहन श्रद्धा, पक्की आस्था तथा सुदृढ़ धारणा की आवश्यकता है, जैसे प्रह्लाद को थी। इसमें पढ़ाई-लिखाई आवश्यक नहीं है। तुकाराम जैसे लोग, जो अपने नाम के हस्ताक्षर तक करना नहीं जानते थे, ने ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। इसके लिए विस्तृत ज्ञान अथवा अध्ययन नहीं चाहिए। भक्त मिठाई खाना चाहता है। वह तो केवल अपने प्रभु का सान्निध्य चाहता है।
ज्ञान आत्म-विस्तारण का योग है। इसमें आत्म निर्भरता की आवश्यकता है। केवल बुद्धि-प्रधान स्वभाव वाले लोग, जो विचार-शक्ति, विवेक-शक्ति तथा तर्क-शक्ति से सम्पन्न हों, ज्ञान-मार्ग के लिए उपयुक्त हैं। यह मर्कटयोग है। बन्दर का बच्चा रोता नहीं, किन्तु उसकी माँ कहीं भी भागती रहे, वह स्वयं ही उसके शरीर के साथ जोर से चिपटा रहता है। इस योग में वेदान्त-साहित्य का विस्तृत अध्ययन, तीक्ष्ण बुद्धि, निर्भीक समझ तथा भीमकाय संकल्प एवं साहस होना चाहिए। ज्ञानी, मिठाई खाने के स्थान पर स्वयं साकार मिठाई ही हो जाना चाहता है। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाना चाहता है।
१४
क्या ज्ञान और भक्ति एक-दूसरे के विरोधी हैं?
मेरा उत्तर है- 'नहीं! बिलकुल नहीं!' वास्तव में इन दोनों में परस्पर नाता है, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। भक्ति ज्ञान का किंचित् भी विरोध नहीं करती। निःसन्देह ये दोनों एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। दोनों एक ही लक्ष्य की ओर ले कर जाते हैं। आप भक्ति को ज्ञान से पूर्णतया अलग नहीं कर सकते। जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो यह ज्ञान में रूपान्तरित हो जाती है। एक वास्तविक ज्ञानी भगवान् हरि का भक्त है, भगवान् कृष्ण का भक्त है; भगवान् राम का, भगवान् शिव का, माँ दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का, ईसा मसीह तथा बुद्ध भगवान् का भक्त है। वह समरस भक्त होता है। कुछ अज्ञानी लोग सोचते. हैं कि ज्ञानी शुष्क होता है तथा उसमें भक्ति बिलकुल नहीं होती। यह बहुत ही दुःखद गलती है। ज्ञानी का हृदय तो अत्यधिक विशाल होता है। श्री शंकराचार्य की भक्तिमय कृतियों को पढ़ कर देखें और उनकी भक्ति की गहराई का अनुमान लगायें। जरा अप्पय्य दीक्षितार की रचनाओं को पढ़ें और उनकी असीम भक्ति की अमित गहराइयों की थाह लेने का प्रयास करें।
स्वामी रामतीर्थ एक ज्ञानी थे। क्या वह भगवान् श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे? यदि कोई वेदान्ती भक्ति का बहिष्कार कर देता है, तो याद रखें, उसने वास्तव में वेदान्त को ठीक से समझा और ग्रहण ही नहीं किया है। एक ही निर्गुण ब्रह्म, थोड़ी-सी माया के सहित सगुण ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों की पावन पूजा ग्रहण करने के लिए अवतरित हो जाता है।
भक्ति ज्ञान से विलग नहीं है। इसके विपरीत ज्ञान भक्ति को प्रगाढ़ करता है। जिस व्यक्ति को वेदान्त का ज्ञान है, वह अपनी भक्ति में भली-भाँति स्थित रहता है। वह सुस्थिर एवं सुदृढ़ हो जाता है। कई अज्ञानी लोग कहते हैं कि यदि कोई भक्त वेदान्त पढ़ लेगा, तो उसकी भक्ति चली जायेगी। यह पूर्णतया गलत है। वेदान्त का अध्ययन तो भक्ति को बढ़ाने और विकसित करने में सहायक है। वेदान्त-साहित्य में प्रवीण व्यक्ति की भक्ति भली-भाँति सुस्थिर हो जाती है। वास्तव में भक्ति और ज्ञान एक पक्षी के दो पंखों की भाँति हैं, जो व्यक्ति को ब्रह्म की ओर उड़ान भरने में, मुक्ति की पराकाष्ठा तक पहुँचाने में सहायता करते हैं।
१५
क्या रात को भोजन करने के बाद ध्यान के लिए बैठना उचित है? सायंकाल के समय तक गृहस्थ व्यक्ति इतना परेशान हो चुका होता है कि उसे ध्यान के लिए समय निकाल सकना ही बहुत कठिन होता है।
सामान्यतया राजसी भोजन करने के बाद लोग निद्रालुता अनुभव करते हैं। आप कल्पना करते रहेंगे कि आप ध्यान में बैठे हैं, किन्तु यह बैठी मुद्रा में पूर्णतया निद्रा भी हो सकती है। यदि आप मिताहार के नियम का अनुसरण करते हैं और सायं ७ बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो आप ९ से १० बजे तक ध्यान के लिए बैठ सकते हैं।
रात्रि के समय ध्यान, अर्थात् दिन में दूसरी बार ध्यान के लिए बैठना निश्चित रूप से अत्यन्त आवश्यक है। यदि आपके पास रात को ध्यान के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता तो आप सोने से पहले कुछ मिनट, अर्थात् १० से १५ मिनट के लिए ध्यान करने के लिए बैठ जायें। इस प्रकार करने से आध्यात्मिक संस्कार विकसित होंगे। यह आध्यात्मिक संस्कार आपके लिए बहुमूल्य निधि हैं। इसके साथ-साथ आपको बुरे सपने नहीं आयेंगे। दिव्य विचार निद्रावस्था में भी चलते रहेंगे। इनका आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
१६
ब्रह्मचर्य का पालन करने में मुझे कठिनाई आ रही है। अचानक ही मैं मूर्खतावश गड्ढे में गिर जाता हूँ। भीतर से मैं वास्तव में दुखी हूँ, किन्तु पशु की भाँति उसी काम में फँस जाता हूँ। क्या करूँ ?
व्रत रखें। किसी एक ही मन्त्र का नित्य तीन घण्टे सतत जप करें। श्रीमद्भगवद्गीता का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ें। अलग कमरे में सोयें। अपने मन को हर समय पूरी तरह व्यस्त रखें। मन को दूसरी ओर मोड़ दें। मन को उदात्त एवं भले विचारों से भर दें। सत्संग करें। थोड़े से कुम्भक सहित, सुखपूर्वक २० प्राणायाम करें। शारीरिक श्रम भी पर्याप्त मात्रा में करें। चिन्तन करें कि आत्मा में न तो काम है, न ही काम वासना ।
१७
मैं बहुत गम्भीरता से ऐसे गुरु की खोज में हूँ, जो सुनिश्चितता से कह सके कि उसने ब्रह्म-साक्षात्कार अथवा भगवद्-दर्शन प्राप्त कर लिया है। क्या आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं? मैं आपसे यह पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ कि क्या आपने ब्रह्म-साक्षात्कार कर लिया है ?
जो प्रश्न आपने पूछे हैं, यह आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले सभी सच्चे साधकों के मन में आने स्वाभाविक हैं। कल्पना कीजिए कि मैं आपसे कह दूँ कि अमुक व्यक्ति ब्रह्म-साक्षात्कार प्राप्त किये हुए है, तो आप मेरे कथन को सत्य-प्रमाणित कैसे करेंगे और इससे आपको लाभ भी क्या होगा ?
साक्षात्कार-प्राप्त आत्माओं का अभाव नहीं है। सामान्य अज्ञानी व्यक्ति सरलता से उन्हें पहचान नहीं सकता। केवल कुछेक लोग, जो शुद्ध हृदय के हैं तथा समस्त सद्गुणों से सम्पन्न हैं,उन्हें समझ सकते हैं, वही उनके सान्निध्य से लाभान्वित हो सकते हैं।
साक्षात्कार-प्राप्त आत्माओं की खोज में इधर-उधर दौड़-भाग करने का कोई लाभ नहीं है। भले ही कृष्ण भगवान् भी आपके साथ रहें, वे भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप उन्हें ग्रहण करने योग्य नहीं बनते। इस बिन्दु को समझें और स्वयं को निष्काम कर्मयोग, दान, धारणा, जप, ब्रह्मचर्य तथा इन्द्रिय-संयम द्वारा शुद्ध करें।
गुरु की परीक्षा करना अत्यन्त कठिन है। यहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें। विश्वास रखें। सच्चा जिज्ञासु इन प्रश्नों और शंकाओं से मुक्त है। यदि आप मेरे कथन पर विश्वास करेंगे, तो आप अद्भुत रूप से लाभान्वित होंगे।
१८
क्या गुरु के लिए अपने शिष्यों को महान् बनाना बहुत कठिन है ?
इस प्रश्न से यह आभास होता है कि गुरु को अपने शिष्यों से अन्य सबकी अपेक्षा अधिक लगाव होता है। यदि ऐसा है, तो वह आध्यात्मिक गुरु नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति की प्रथम योग्यता, आसक्ति पर विजय प्राप्त होना है। वास्तविकता यह है कि सहस्रों में से कोई एक-दो विरले ही इस योग्यता को प्राप्त कर पाते हैं और केवल वही व्यक्ति महान् हैं, महामानव हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लोग चारों ओर से घेरे रहते हैं, जो उसके अन्तरनिहित आकर्षण से प्रभावित होते हैं। किन्तु जो लोग उन्हें घेरे रहते हैं, उनमें गुरु होने की योग्यता नहीं होती। वह तो सामान्य लोग ही होते हैं।
१९
एक असामान्य महिला ने दश वर्षों तक निरन्तर कठोर योगानुशासन में रहते हुए एक महानतम योगगुरु के पास अध्ययन किया और अन्ततः वह इस नतीजे पर पहुँची कि यह सब-कुछ भ्रम है, मृगतृष्णा है।
आपने उस महिला के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, उससे ज्ञात हो जाता है कि उसमें वह योग्यता नहीं थी कि किसी से लाभान्वित हो सके, भले ही वह व्यक्ति भगवान् बुद्ध जैसी आध्यात्मिक उन्नति तक पहुँचा हुआ क्यों न हो। आध्यात्मिक विकास के लिए एक वस्तु, जो बहुत आवश्यक है, वह है-अध्यवसाय अथवा दृढ़ता। वह स्वयं को तरह-तरह की कृतियों से भरती जा रही थी और सभी उसे अलग-अलग रास्ते बतलाने वाली थीं। यदि कोई व्यक्ति कुआँ खोदना चाहता है तो उसे एक ही स्थान पर निरन्तर खुदाई करनी पड़ेगी, जब तक कि वह पानी तक नहीं पहुँच जाता है। यदि वह सौ स्थानों पर खुदाई करे और हरेक गड्डा पाँच फुट से कम गहरा खोदे बिना ही छोड़ दे, तो वह कभी कुआँ नहीं खोद पायेगा। उस महिला की यही स्थिति थी। उसकी धारणा को क्या महत्त्व दिया जा सकता है?
२०
तीर्थयात्रा को इतना पावन क्यों माना जाता है, पर्यटन अथवा कार्यालय सम्बन्धी यात्रा को क्यों नहीं?
क्योंकि, 'तीर्थयात्रा पर जाना है', यह विचार आते ही आपका मन आपको एक अलग ही उच्चतर एवं भक्तिपूर्ण भाव में ले जाता है। मन के सांसारिक घुमाव बन्द होने लगते हैं। जब आप अपने शहर को छोड़ कर निकलते हैं, तो आप अपने सामाजिक जीवन के बोझिल आवरण को निकाल फेंकते हैं। आप भले ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा पर निकले हों, धीरे-धीरे आपको लगने लग जाता है कि वे सब आपके सगे-सम्बन्धी इतने नहीं हैं, जितने कि सह तीर्थयात्री हैं। और यदि आप अकेले हैं, तो आप सम्भवतया पारिवारिक चिन्ता एवं तनाव से मुक्त तथा पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत् में रहते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है, जो उत्तराखण्ड जैसे पावन क्षेत्रों के चतुर्दिक् व्याप्त आध्यात्मिक तरंगों को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया अनुकूल है। जो व्यक्ति तीर्थयात्री होने के भाव से तीर्थस्थान पर जाता है, वह इस बात के प्रति जागरूक होता है कि वह आध्यात्मिक अनुभव-प्राप्ति के पावन लक्ष्य को ले कर निकला है, इसलिए उसे इस यात्रा से महान् लाभ प्राप्त होगा और जब वह यात्रा से लौटेगा तो वह पूर्णतया परिवर्तित व्यक्ति होगा।
२१
तीर्थयात्रा से लोग कैसे लाभान्वित होते हैं?
इस प्रश्न का उत्तर तो प्रत्येक तीर्थयात्री को अपने बारे में स्वयं ही बताना होगा। आध्यात्मिक लाभ सदैव हृदय के विश्वास पर निर्भर करता है। विश्वास मनुष्य की आत्मा का प्राण है। इसके बिना कोई भी आध्यात्मिक साधना सफल नहीं हो सकती। और इसके साथ, कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति असम्भव नहीं है। यदि तीर्थयात्री को मन में विश्वास हो, उसकी धारणा दृढ़ हो और निश्चय पक्का हो कि उसके समस्त पाप धुल जायेंगे, कि उसे मोक्ष प्राप्ति हो जायेगी तथा वह संसार-चक्र से निकल जायेगा, तो फिर ऐसा बिलकुल भी कोई कारण नहीं है कि यह सत्य सिद्ध न हो। बद्री केदार जैसी तीर्थयात्रा आपके समस्त पापों को धो देती है तथा आपको इस योग्य बना देती है कि आप जीवन के परम लक्ष्य-ईश्वर-साक्षात्कार (यदि इसकी महिमा में निष्ठा है, तो) की ओर अग्रसर होने लगें। किन्तु याद रखें, आपके इस विश्वास का परीक्षण यह है कि जब आप यात्रा से लौटते हैं, तब कैसे हैं; यदि यात्रा से लौटने पर आप यह सिद्ध कर देते हैं कि आपने अपने समस्त पाप पूर्णतया धो डाले हैं, कि अपने सारे कुसंस्कार पावन नदियों के जल में स्नान करके बहा डाले हैं, कि जिस उदात्त वातावरण में आप घूम कर आये हैं, उसकी आध्यात्मिक तरंगों से आप पूरी तरह से भर गये हैं तथा यदि आपने एक सही, भक्तिपूर्ण, सत्यपरायण और पवित्र जीवन जीना आरम्भ कर दिया है, तो आप निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेंगे। तब तीर्थयात्रा ने अपना उद्देश्य पूर्ण कर दिया समझें।
कुछ तीर्थयात्री (भले ही बहुत कम संख्या में हैं, और प्रकट भी नहीं करते हैं, किन्तु फिर भी) ऐसे हैं, जो तीर्थयात्रा द्वारा आध्यात्मिक ऊँचाइयों तक पहुँच जाते हैं।
२२
'माई मैगजीन' में मैंने आपका लेख पढ़ा, “सांसारिक मन वाले लोगों का साथ छोड़ दो। सांसारिक बातें करने वाले आपके मन को दूषित कर देंगे। आपका मन चंचल हो जायेगा। दौड़ें ! भागें ! ऋषिकेश जैसे एकान्त स्थानों में भाग जायें! आप आध्यात्मिक पथ पर सुरक्षित रहेंगे।" क्या मैं आपके पास आ कर संन्यासी-जीवन बिता सकता हूँ?
उतावले न बनें। भली-भाँति सोचें। पहले तोलें, फिर बोलें। आध्यात्मिक मार्ग में केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा। उपरोक्त निर्देशन उन लोगों के लिए हैं, जो पहले से ही किसी-न-किसी साधना में लगे हुए हैं। उनको उच्चतर साधना के लिए एकान्त में जाना पड़ेगा। आप जैसे प्रारम्भिक साधकों के लिए संसार में रहते हुए, रोगियों और वृद्धों की तीन वर्ष निरन्तर निःस्वार्थ कर्मयोग की साधना करना अधिक अच्छा रहेगा।
मान लें कि आप संन्यासी हो कर मेरे पास रहते हैं, तो क्या आपमें इतनी शक्ति है कि यदि आपकी माता जी आ कर आपके सामने भग्नहृदय से फूट-फूट कर रोने लगें, तो आप उनका सामना कर सकेंगे? यदि आपके पिता जी आपको आ कर धमकाने लगें, तो क्या आप इस पथ पर दृढ़ रह सकेंगे? यदि कोई युवती आपको प्रलोभित करे, तो क्या आप अप्रभावित रहेंगे! यदि आप किसी रोग से ग्रसित हो जायें, तो क्या इस पथ पर दृढ़ रह सकेंगे? क्या आप सत्य-पथ पर अपना शरीर और जीवन न्योछावर करने को तैयार हैं? क्या आपने संन्यास एवं एकान्त की महिमा को जान लिया है? संन्यासियों को जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आप दर-दर भटक कर भिक्षा-वृत्ति द्वारा निर्वाह करने के लिए तैयार हैं? जब आपको निर्जन स्थान में रहना पड़ेगा तो आप पूरा दिन और रात कैसे बितायेंगे? यहाँ आने से पहले इन सब बातों पर भली-भाँति विचार कर लें। यदि आपको पूरा विश्वास है कि आप संन्यास के लिए तैयार हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। मैं आपकी अच्छी तरह देखभाल करूँगा और सहायता करूँगा। मैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान रखूँगा। मैं आपको शाहों का शहंशाह बना दूंगा। त्यागमय जीवन से बढ़ कर सुखदायक जीवन और कोई नहीं है। शीघ्र ही आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त है। संन्यासियों की जय हो!
२३
मैं-जो ब्रह्म हूँ, परम चैतन्य हूँ, अद्वितीय, अनन्त, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् हूँ, मुझे प्रकृति को प्रकट करने की आवश्यकता ही क्या है? मुझे प्रकृति के नियमों में बँधना और देश, काल एवं कारण की सीमाओं में सीमित होना क्यों आवश्यक है और सबसे बढ़ कर, मुझे क्रम-विकास एवं प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया के चक्र में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है?
आँख अपने-आपको नहीं देख सकती। मनुष्य अपने कन्धों पर स्वयं सवार नहीं हो सकता। इसी तरह उस परम तत्त्व के, समस्त सृष्टि के कारण-रहित कारण के विषय में की जाने वाली सारी खोज आदि-अज्ञान से जा टकराती है। जो व्यक्ति अपनी मैं को शून्य तक ले जाता है, और इस प्रकार जो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेता है, वह इस दीवार को भेद कर उस अनन्त के साम्राज्य में प्रवेश पा जाता है। तब वह सब जान जाता है। किन्तु यह जानकारी किसी अन्य को बतायी नहीं जा सकती, क्योंकि इस विशाल दीवार ने दूसरों को सत्य जानने से रोक कर रखा हुआ है। इसलिए प्राचीन सन्तों ने इसे अतिप्रश्न कहा है।
केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि भगवान् ने इस सृष्टि की रचना इसलिए की है कि आप स्वयं को विकसित कर सकें और आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर सकें, ताकि आप उनके प्रकटीकृत रूप-इस समस्त सृष्टि की सेवा कर सकें और उससे प्रेम कर सकें। अज्ञान रूपी डाकू ने मनुष्य को आत्म-जागरूकता के अपने महल से अपहृत कर लिया है और उसे घने जंगल में ला पटका है। जब वह जागता है तो वह यहाँ कैसे आ गया, इसकी चिन्ता नहीं करता, अपितु यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसी प्रकार, सच्चा साधक आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करके जन्म-मरण के चक्र से निकलने का प्रयास करता है।
२४
वे सर्वहितैषी, दया के सागर, करुणा-सिन्धु भगवान् सदाचारी व्यक्ति की सहायता क्यों नहीं करते और उसे सुखी क्यों नहीं रखते ? वे उसे पूर्व-जन्म के कर्मों की दया पर क्यों छोड़ देते हैं?
कर्म एक पहिये की भाँति होते हैं। उनको पूरा करना ही पड़ता है। जिस शक्ति से वह गति में आये होते हैं, उसे खर्च करना ही पड़ता है। यह क्रिया एवं प्रतिक्रिया का चक्र है। जैसे धनुष से एक बार छूटा हुआ बाण वापस नहीं लौटाया जा सकता भले ही शिकारी को यह लगे कि उसने गलत जगह निशाना लगा दिया है; इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म, अर्थात् गत जन्मों के किये गये कर्मों के फल जो परिपक्व हो कर इस जन्म में भोगने के लिए आ गये हैं, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता
फिर भगवान् अपने भक्त की सहायता कैसे करते हैं? वह करुणा-सागर प्रभु उसकी संकल्प-शक्ति को सुदृढ़ करके तथा सहन-शक्ति को बढ़ा कर, प्रसन्नतापूर्वक कर्म-फल भोगने की शक्ति दे कर सहायता करते हैं। निश्चित रूप से भक्त को पूर्व-कर्मों की दया पर नहीं छोड़ दिया जाता। वह उनके द्वारा अपनी दया के सुरक्षा-कवच से भली-भाँति आवृत्त कर दिया गया होता है। जिस प्रकार भीषण जाड़े और प्रचण्ड वायु में आप अपने घर में एवं गर्म कपड़ों में सुरक्षित रहते हैं, इसी प्रकार भगवान् का भक्त (भले ही देखने वालों को वह अकिंचन, रोगी और पीड़ित प्रतीत होता हो) यह अनुभव नहीं करता कि वह जरा-से भी कष्ट में है और वह सदा उनके स्मरण में प्रसन्न एवं आनन्दित रहता है।
२५
गलत काम करने वाला व्यक्ति तर्क देता है कि वह अपने कर्मों के कारण यह सब कर रहा है, और वह ऐसा न करने का भी प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा करने में प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसे कैसे समझाया जाये कि ऐसे न करे ?
कर्म मनुष्य को गलत कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करता। हाँ, संस्कार कुछ हद तक करते हैं। भगवान् ने मानव को स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति प्रदान की है, जिससे वह अपने भविष्य को बिगाड़ या सँवार सकता है। मनुष्य को भोग-स्वतन्त्रता नहीं है, जो कि कर्म द्वारा संचालित है। किन्तु उसे कर्म-स्वतन्त्रता है। वह अपने कुसंस्कारों को विचार-शक्ति द्वारा, इच्छा-शक्ति द्वारा और भले कार्यों के सतत अभ्यास द्वारा सुसंस्कारों में बदल सकता है।
दुर्गुण तत्काल सुख देते प्रतीत होते हैं, यही सबसे बड़ा लोभ है और यही सद्गुण अर्जित करने में सबसे बड़ी बाधा है। इसका निराकरण केवल विवेक एवं अनुभव द्वारा हो सकता है। परमात्मा का ध्यान करने से तथा दुष्कर्मों के कारण उस व्यक्ति की आत्मा को एवं समस्त समाज को होने वाली हानि का चिन्तन करने से व्यक्ति दुष्कर्म करने से बच सकता है, किन्तु तत्काल सुख प्रतीत होने वाले दुष्कर्म उसे फिर लुभा लेते हैं। इस गम्भीर समस्या का हल सुगम नहीं है, दुष्टहृदयी इतने शीघ्र नहीं बदलता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सत्संग को इतना बढ़ावा दिया। केवल विद्वज्जनों एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत सन्तों का सतत संग ही दुष्टों के मन से गलत धारणाओं को निकाल सकता है।
२६
मैं एक अनजान स्त्री हूँ, जो कभी आपसे मिलेगी-इसकी आपने कभी कल्पना भी न की होगी, किन्तु मेरी प्रार्थना है कि स्त्री होने के कारण आप मुझसे घृणा न करें! मैं तो केवल आध्यात्मिक जीवन का आनन्द पाने को लालायित हूँ। स्वामी जी, स्त्री होने पर भी कृपा करके मेरी ओर ध्यान दें और मुझे बतायें कि क्या मैं ऐसे आनन्द को प्राप्त कर सकूँगी ? और यदि हाँ, तो ऐसा कब होगा ?
कहते हैं कि व्यक्ति के सही गुरु होना अनिवार्य है; किन्तु मैं नहीं जानती कि ऐसे गुरु को मैं कहाँ खोजूँ जो मेरी इस क्षुधा को शीघ्र तृप्त कर दे। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं?
क्या आपके गुरु थे ? कौन थे वह ? कृपया मुझे उनके विषय में बतायें। यदि मैं धृष्टता नहीं कर रही हूँ, तो कृपया बतायें कि क्या वह सद्गुरु थे, या हैं?
क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको गुरु अथवा सद्गुरु कहा जा सकता है?
मुझे यह जान कर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप आध्यात्मिक जीवन का आनन्द प्राप्त करने को अत्यधिक लालायित हैं। आपके संस्कार अच्छे एवं आध्यात्मिक हैं। इनको सुरक्षित रखें। नियमित अभ्यास के द्वारा आप आध्यात्मिक आनन्द को प्राप्त कर सकती हैं।
मैं किसी से भी घृणा नहीं करता। महिलाओं में मैं निज आत्मस्वरूपवत् श्रद्धा रखता हूँ। नारी महाशक्ति का प्रकटीकृत रूप है। मैं उसकी दुर्गा अथवा काली के रूप में उपासना करता हूँ। यद्यपि स्त्रियों को अबला (बलहीन) कहते हैं, तथापि वे इस धरा पर सक्रिय शक्तिस्वरूपा हैं। धर्म की सुरक्षा केवल उन्हीं के माध्यम से हो रही है। भारतीय नारियों में भक्ति का तत्त्व अन्तर्निहित है। उनमें अविचल भक्ति होती है। यदि वे निश्वय कर लें, तो परमात्म-साक्षात्कार अति शीघ्र प्राप्त कर सकती हैं।
क्या आप मीरा के समान नहीं होना चाहतीं ? यदि आपका मन सचमुच ईश्वरोन्मुख हो चुका है, यदि आप अपनी आध्यात्मिक साधनाओं में गम्भीर और सुदृढ़ हैं, तो बहुत शीघ्र ही आप दिव्य आनन्द प्राप्त कर सकती हैं। आनन्दित हो जायें! निर्भीक बनें! सुदृढ़ रहें! स्वयं को पहचानें ! साक्षात्कार प्राप्त करें! आध्यात्मिक आनन्द का आस्वादन करें!
यदि आपकी इच्छा वास्तविक है तो गुरु आपको अपने समक्ष प्राप्त हो सकता है। सच्चे जिज्ञासु दुष्प्राप्य हैं। हाँ, मेरे भी गुरु हैं। स्थान का अभाव होने के कारण, मैं उनकेविषय में विस्तार से नहीं बता सकता। मैं, न तो गुरु हूँ, न ही सद्गुरु। दूसरे की सेवा करने में मुझे आनन्द प्राप्त होता है। मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा को तत्पर हूँ, तथा मेरे पास जो कुछ भी है, वह आपसे बाँटने को तैयार हूँ। मैं आपके संशयों का निवारण करके आपको अध्यात्म-पथ पर अग्रसर कर दूँगा।
२७
क्या गुरु या शिक्षक के निर्देशन की सहायता लिए बिना प्राणायाम का अभ्यास करने में खतरा है ?
साधारण प्राणायाम का अभ्यास गुरु की सहायता के बिना किया जा सकता है। यदि आप सतर्क हैं और सहज बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो आसन-प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करने में कोई खतरा नहीं है। लोग अकारण ही भयभीत रहते हैं। यदि आप लापरवाह हैं, तो प्रत्येक कार्य करने में खतरा है। यदि आप लापरवाही से सीढ़ी उतरते हैं, तो आप गिर कर टाँग की हड्डी तुड़वा बैठेंगे। जब आप अपने शहर के किसी व्यस्त क्षेत्र में से जा रहे होते हैं, उस समय यदि आप लापरवाही से चलते हैं, तो गाड़ी के नीचे आ कर कुचले जाने का भय रहेगा। यदि आप स्टेशन पर टिकट लेते समय सतर्क नहीं रहते, तो अपना बटुआ गंवा बैठेंगे। यदि दवाइयों के मिश्रण बनाते समय सतर्क नहीं हैं, रोगियों को गलत दवाइयाँ अथवा विष या आवश्यकता से अधिक खुराक दे कर, उनके प्राण ले लेंगे। इसी प्रकार जब आप प्राणायाम करते हैं, तो आपको अपने भोजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पेट को बहुत अधिक भर कर नहीं खाना चाहिए, आपको हल्का, शीघ्र पचने वाला और शक्ति देने वाला भोजन करना चाहिए। आपको सम्भोग में संयमित होना चाहिए। पहले आपको कुम्भक के बिना, एक या दो मास तक केवल अनुलोम-विलोम करना चाहिए, फिर धीरे-धीरे श्वास-प्रश्वास के अनुपात को १:४:२ से बढ़ाते हुए, १६:६४:३२ तक ले जाना चाहिए। साँस को बहुत धीरे-धीरे छोड़ें। यदि इन नियमों का पालन किया जाये, तो प्राणायाम का अभ्यास करने में कोई भय नहीं है।
यदि आप दीर्घ काल तक कुम्भक करने का अभ्यास करना चाहते हैं तथा अपान को प्राण से मिला देना चाहते हैं, तब गुरु का होना आवश्यक है। यदि गुरु नहीं मिल रहा तो साक्षात्कार प्राप्त योगियों की पुस्तकें आपको निर्देशन दे सकती हैं। किन्तु गुरु के पास होना अधिक अच्छा है। या आप उनसे निर्देशन प्राप्त करके अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं। उनसे नियमित पत्र-व्यवहार करते रह सकते हैं। आधे या एक मिनट तक तो आप बिना किसी कठिनाई या भय के कुम्भक कर सकते हैं। यदि कोई साक्षात्कार-प्राप्त योगी नहीं मिलता, तो आप योग के वरिष्ठ विद्यार्थी के पास जा सकते हैं। वे भी आपकी सहायता कर सकते हैं।
२८
क्या आहार-शुद्धि से मन पवित्र होता है? क्या निरामिष भोजन सात्त्विक नहीं है ? महाभारत में हमें लोगों द्वारा यज्ञ में समर्पित बलि के बकरे खाये जाने के उदाहरण मिलते हैं।
हाँ, भोजन की शुद्धि से मन शुद्ध होता है। 'आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः ।' शैम्पेन (मदिरा) की एक खुराक लें और ध्यान में बैठ कर देखें। सन्तरे के रस की एक खुराक पियें और ध्यान के लिए बैठें। आपको अन्तर पता चल जायेगा। अलग-अलग प्रकार का भोजन, मस्तिष्क के अलग-अलग भागों पर प्रभाव डालता है। मदिरा पीने, माँस और लहसुन खाने hat H . जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो आपका मन चंचल एवं परेशान रहेगा। दूध और फल लेने से आप मन को भली-भाँति एकाग्र कर लेंगे। हमारे ऋषि-मुनि दूध और फलों पर ही रहते थे। छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है, आहार शुद्धि से मन शुद्ध होता है और तब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको आहार-संयम रखना चाहिए।
मांसाहार सात्त्विक नहीं है। साधक के लिए यह अच्छा नहीं है। एक मास तक दूध और फलों पर रहें और फिर देखें। हमें करके देखना चाहिए। करने से आपको अनुभव हो जायेगा कि निरामिष भोजन करना मन के लिए ठीक नहीं है।
२९
इनमें से क्या अधिक अच्छा है? गृहस्थ-जीवन व्यतीत करना या संन्यासी हो जाना ?
आप एकदम से संसार का त्याग नहीं कर सकते। संसार एक विशाल विश्वविद्यालय है। प्रकृति सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। संसार में रह कर आप दया, सहन-शक्ति इत्यादि सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। एकाकी गुहाओं में रह कर आप इनका विकास नहीं कर सकते। संसार सर्वोत्तम गुरु है। धीरे-धीरे जब आप उन्नत स्थिति प्राप्त कर लेंगे, तब संन्यास ले सकते हैं। गुरु नानक संसार में ही रहे। उनके दो पुत्र थे। संसार में रहने में कुछ गलती नहीं है। प्रार्थना सब कठिनाइयों को दूर कर देगी।
३०
कहीं-कहीं ऐसा सुना है कि साधु और संन्यासियों के साथ मित्रता करने से व्यक्ति का बहुत कुछ बन या बिगड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्ध सन्त की भावना को आहत करता है, तो कहते हैं कि वह उसे शाप दे देता है और उसे बहुत-सी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। यह कहाँ तक सच है ?
साधु एवं संन्यासियों का साथ सदा ही मनमोहक है, यदि वह उत्तम चरित्र से सम्पन्न हैं तो! यदि यही एकमात्र गुण उनमें विद्यमान है तो वे पूजा और सम्मान पाने के पूर्ण अधिकारी हैं। वे कभी भी किसी को कष्ट पहुँचाने का कारण नहीं बन सकते।
सच्चे साधु और संन्यासियों का सम्पर्क कभी भी लोगों की उन्नति में बाधा का अथवा उनकी निजी हानि का कारण नहीं हो सकता। साधु तो उनको सही एवं नैतिक नियमों का पालन करने योग्य बनने में सहायता करते हैं। साधु-सन्तों के आशीर्वाद लोगों के लिए अनमोल धन हैं। सांसारिक बुद्धि से सम्पन्न लोगों के मन स्वभावतया जिन कुसंस्कारों से भरे होते हैं, साधु-सन्तों का संग उन्हें शुद्ध करने में सहायता करता है।
ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त सन्त को भले ही कितना उकसाने का प्रयत्न किया जाये, वह कभी भी किसी को शाप नहीं देता; बल्कि सर्वशक्तिमान् परमात्मा से प्रार्थना करता है-उसे खतरों एवं अपमान से बचाने के लिए नहीं, अपितु उसे और उसके विरोधियों को भी ज्ञान, प्रकाश, पवित्रता एवं द्युति प्रदान करने के लिए। उसे चोट पहुँचाये जाने पर भी
वह कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाता। वह अत्यन्त सहज रूप से क्षमा करके उसे भूल जाता है। वह अपने प्रति किये गये किसी भी अनुचित कार्य को याद नहीं रखता। सच्चा ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त सन्त चोर, लम्पट, कपटी, हत्यारा, आक्रामक, चींटी, श्वान, अछूत, ब्राह्मण, पेड़, पाषाण, बिच्छु यहाँ तक कि इस समस्त जड़-चेतन सृष्टि में अपने इष्ट की छवि को देखता है। वह सबके साथ स्वयं को एक ही देखता है। जब यह स्थिति है कि वह सबको आत्मवत् ही देखता है, तो वह किसे शाप दे सकता है?
याद रखें कि वह साधु या संन्यासी ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति नहीं हो सकता जो किसी भी कारण से किसी को शाप देता है। यह भी सच है कि कोई पवित्रात्मा (भले ही वह साधु या संन्यासी न भी हो) यदि शारीरिक या मानसिक कष्ट के प्रभाव से किसी को शाप दे दे तो वह तत्काल फलित हो जाता है।
३१
जब गुरु और भगवान् - दोनों की कृपा है, तब फिर मन नियन्त्रित क्यों नहीं होता ?
इसके साथ-साथ पुरुषार्थ भी अत्यन्त आवश्यक है। जब आप पुरुषार्थ करते हैं, केवल तभी कृपा होती है। कोई प्राध्यापक आपके लिए प्रश्नों के उत्तर लिख कर आपको सफलता नहीं दिलवायेगा। गीता कहती है, 'उद्धरेदात्मनात्मानम्।' व्यक्ति को स्वयं अपने-आपको उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। कृपा व्यक्ति को उन्नत होने में सहायता करती है। प्रत्येक को अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वयं परिश्रम करना चाहिए। आप पूछेंगे कि फिर कृपा क्या है? यदि साधक को अपने गुरु के पत्र प्राप्त होते हैं और उनसे उसकी समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है, वह कृपा है। यदि कोई साधक यहाँ आ जाता है और गंगा स्नान कर लेता है, तो यह कृपा है। अनेकों इसके लिए लालायित हैं। यहाँ तक कि कितने ही करोड़पति यहाँ आने और गंगा स्नान करने के लिए तरसते रहते हैं, किन्तु उन्हें एक बार भी आ कर अपनी इच्छा-पूर्ति का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। यदि स्वाध्याय के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो यह कृपा है। यदि किसी का स्वास्थ्य इतना अच्छा है कि वह साधना कर सके, तो यह कृपा है। यदि भगवान् चाहें तो एक ही बार में झट से सारे जगत् को मुक्ति दे सकते हैं, किन्तु वे ऐसा नहीं करते, उनकी कृपा-वृष्टि वहीं होती है, जहाँ पुरुषार्थ होता है।
३२
भगवान् ने यह संसार क्यों बनाया है?
भगवान् से पूछें कि उन्होंने यह संसार क्यों बनाया है? आत्म-ज्ञान प्राप्त करें। तब आप जान लेंगे कि भगवान् ने संसार क्यों बनाया है। आप अपनी बुद्धि से यह नहीं समझ सकते। केवल अन्तर्ज्ञान द्वारा ही आप इसे जान सकते हैं।
भगवान् ने लीला के लिए संसार की रचना की है, "लोकवत् तु लीला कैवल्यम्।" सृष्टि की रचना के पीछे कुछ उद्देश्य है। जिस तरह किरणों के बिना सूर्य नहीं होता, उसी तरह सृष्टि-क्रम के बिना भगवान् भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। संसार सूर्य की किरणों की तरह है। यह उनकी प्रकृति है। जैसे जादूगर अपने माया जाल से कुछ वस्तुएँ बनाता है और फिर अन्य कुछ वस्तुओं को गायब कर देता है, इसी प्रकार भगवान् भी इस संसार की रचना कर देते हैं और फिर अपनी लीला से उसे विलीन कर देते हैं। भगवान् सर्वव्यापक हैं। भगवान् ने संसार कब और क्यों बनाया, यह प्रश्न अति-प्रश्न है, दुर्बोध प्रश्न है। इस सम्बन्ध में तर्क-वितर्क करने से हम अपना समय ही नष्ट करेंगे। संसार के विषय में पूछने से पहले, अपने विषय में पूछें, अपने-आपको जानें। इसे जान लेने से आप सब-कुछ जान जायेंगे।
३३
औद्योगिक क्रान्ति के कारण नैतिक नियमों एवं नैतिक स्तर के पतन का क्या कोई इलाज है?
औद्योगिक क्रान्ति किसी को बाध्य नहीं करती कि नैतिक स्तर को गिराया जाये। इसमें तो सन्देह नहीं है कि कुछ हद तक तो इसने पतन को बढ़ावा दिया है; किन्तु मुख्य हाथ मानवता को आध्यात्मिक मूल्यों की अपेक्षा भौतिक प्रसाधनों के मूल्यों को जान-बूझ कर श्रेष्ठ सिद्ध करके गलत दिशा-निर्देश देने वालों का है। अब भी यदि मनुष्य अपने मन से स्थूल स्वार्थपरता को निकाल कर शुद्ध कर लेता है तथा उसमें स्व-विकसन एवं सदाचरण को स्थापित कर लेता है तो इतने अधिक औद्योगिक विकास के रहते हुए भी उच्चतर नैतिक स्तर को बनाये रखा जा सकता है।
३४
इस संसार के जीवन की क्षणभंगुरता को देखते हुए भी मनुष्य मृत्यु को याद क्यों नहीं रखता और पाप-कर्म करना क्यों नहीं छोड़ता ?
प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में पहले-पहले अचानक मनुष्य बन कर नहीं आ जाता। संसार में जीव जब से इस सृष्टि-क्रम में प्रवेश करता है, तभी से एक या दश या सौ अथवा सहस्रों बार नहीं, बल्कि लाखों-लाखों बार जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त होता हुआ निरन्तर जन्म-मरण के चक्र में पड़ा रहता है। वास्तव में वह प्रत्येक जन्म में भोगे हुए कर्म-फलों के संस्कार वर्तमान जन्म तक साथ लिये रहता है। अनभोगे अथवा शेष बचे संस्कार तब तक साथ चलते ही रहते हैं, जब तक कि आत्मज्ञान की अग्नि से पूरी तरह भस्मीभूत नहीं कर दिये जाते। यद्यपि मनुष्य नित्य ही लोगों को मरते हुए देखता है, फिर भी उसका अज्ञान, उसे सत्य को स्वीकारने नहीं देता। अब तक जो अनुभव उसने प्राप्त किये होते हैं, वह अभी इतने पर्याप्त नहीं होते कि उसका ध्यान 'शाश्वत सत्य' अर्थात् परमात्मा की ओर खींचें, किन्तु एक दिन ऐसा निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आयेगा, जब किसी दुर्लभ गुण के द्वारा (वह चाहे महात्माओं के साथ सत्संग के द्वारा हो, गुरु-भक्ति से हो या प्रभु कृपा से हो) वह अन्ततः धीरे-धीरे विकसित होता हुआ परम सत्य की ओर उन्मुख होगा।
मनुष्य अधिकतर अज्ञान से प्रेरित हुआ पाप-कर्म की ओर अग्रसर होता है। जब निःस्वार्थ भले कार्यों को करने से, जप-स्वाध्याय इत्यादि से तथा गुरु-कृपा से अज्ञान सदा के लिए समाप्त हो जाता है, तब परम लक्ष्य सदैव आँखों के सामने रहने लगता है। पाप-कर्मों में प्रवृत्त होना यह संकेत करता है कि जीव अभी विकास को प्राप्त नहीं हुआ है, कि अभी उसे संसार में रह कर और अनुभव प्राप्त करने हैं तथा अभी और निरन्तर स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होना है। अज्ञान को दूर हटाने के लिए तथा भगवान् का सतत स्मरण बने रहने के लिए संसार के कठोर आघात ही सबसे बड़े साधन हैं।
३५
वास्तविक और सच्ची महानता जानने के लिए क्या मानदण्ड हैं?
व्यक्ति की सच्ची वास्तविकता उसके पास होने वाली धनराशि से अथवा कोठियों एवं कारों से अथवा उच्च पद से नहीं आँकनी चाहिए; बल्कि उसके निःस्वार्थता, सर्व-प्रेममय दृष्टिकोण, हृदय की विशालता, उदार विचार, विश्वहित, आत्म-बलिदान, निरहंकारिता, आत्म-विलोपनता, अनेकता में एकता देखने की मात्रा, मानवीय सेवाएँ इत्यादि के गुणों से परखनी चाहिए। वास्तविक महान् व्यक्ति पवित्र होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होता है, उदारचित्त एवं उदारहृदयी होता है। वह कभी भी अपने ही लिए नहीं सोचता तथा अपने निजी भले, स्वार्थपरता एवं व्यक्तिगत लाभों को एक तरफ हटा कर मानव मात्र की भलाई में ही तत्पर रहता है। वह मानवता की भलाई के लिए प्रार्थना करता है। जहाँ खुला, विशाल, असंकुचित हृदय है वहीं पर वास्तविक महानता है।
३६
धर्मपरायण व्यक्ति कौन है?
जो काया, वाचा, मनसा पवित्र है तथा जो यम एवं नियमों का अक्षरशः पालन करता है। संगीन के सामने होने पर भी वह अपने धर्म पर अडिग रहता है। छोटे-छोटे तुच्छ लाभों और स्वार्थों के लिए वह कभी भी सदाचरण से विचलित नहीं होता। वह सदैव पवित्र, भगवान् का भय मानने वाला, आत्म-संस्थित तथा निःस्वार्थी होता है। वह विश्वहित का सोचने वाला एवं उदार दृष्टिकोण वाला होता है। वह सबके प्रति धीर और सहनशील होता है। वह दानशीलता, सादगी, उदात्तता, गम्भीरता, विनम्रता, त्याग, शान्ति इत्यादि समस्त सद्गुणों की खान ही होता है। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, चतुराई तथा दम्भ इत्यादि दुर्गुणों से वह पूर्णतया परे रहता है। ऐसा नेक एवं धर्मपरायण व्यक्ति सभी की श्रद्धा का पात्र है। उसका कभी भी कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह मित्र-शत्रु-सभी से समान रूप से प्रेम करता है।
३७
कोई भी व्यक्ति अपनी युवावस्था को दीर्घ काल तक स्थायी कैसे रख सकता है ?
इसके लिए योग-पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। चिकित्सा के अन्य सभी प्रचलित साधनों से यह श्रेष्ठ एवं सस्ती है। उत्साहपूर्वक प्राणायाम और आसन करें। ये दोनों वीर्य को सुरक्षित रखने तथा शक्ति को ओजस में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, पश्चिमोत्तान आसन, पादहस्तासन तथा योगमुद्रा के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। जब तक 'केवल कुम्भक' की स्थिति तक न पहुँच जायें, तब तक प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। जब श्वास लेने अथवा छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वीर्य स्थिर हो जाता है; अर्थात् किसी भी रूप में वीर्य-पतन नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधि 'च्यवनप्राश' का निरन्तर सेवन करते रहने से युवावस्था बहुत दीर्घ काल तक बनी रहती है।
३८
'शिवा'ज़ ट्रेजर' नामक रचना में 'आर यू रीयली क्वालिफाइड ?' नामक शीर्षक लेख के पैरा ३ में आपने लिखा है, "यदि इसे (साधक को) कोई वस्तु देने से इन्कार कर दिया जाये, तो उसे उस वस्तु के प्रति इच्छा ही समाप्त कर देनी चाहिए।" क्या यह कथन झूठी आत्म-तुष्टि को प्रोत्साहन देना तथा पराजित मानसिकता को बढ़ावा देना नहीं है? कृपया इस असंगति का समाधान करके कृतार्थ करें।
"यदि उसे (साधक को) कोई वस्तु देने से इन्कार कर दिया जाये तो उस वस्तु के प्रति उसे पुनः इच्छा ही नहीं करनी चाहिए।"
इस कथन को तब तक बार-बार पढ़ते जायें, जब तक यह आपके सम्पूर्ण व्यक्तित्व में व्याप्त न हो जाये, जब तक इसका सही सार-तत्त्व पूरी तरह आपके भीतर न उतर जाये। केवल तभी इसके पीछे निहित महान् सत्य के सही भाव को आप समझ पायेंगे। 'न चाहो, न ठुकराओ' - एक आदर्श साधक का यह आदर्श-वाक्य होना चाहिए।
उसे किसी भी वस्तु-विशेष के प्रति ललक, चाहना अथवा लगाव नहीं होना चाहिए, भले ही वह उसकी कितनी ही मनभाती वस्तु क्यों न हो। जो कुछ भी बिना किसी प्रयास के संयोगवश उसे मिल जाये, (बस वह उसके नैतिक स्तर को गिराने वाला न हो, तो) उसका साधक को स्वागत करना चाहिए। उसे किसी भी वस्तु-पदार्थ के प्रति लगाव इसलिए नहीं होना चाहिए; क्योंकि दैव-इच्छा से वह वस्तु यदि उससे अलग कर दी जाये, तो उसे मानसिक क्लेश झेलना पड़ सकता है। प्रत्येक वस्तु का व्यक्ति को प्रभु-इच्छा से ही संयोग अथवा वियोग होता है, भले ही मनुष्य ने उसके लिए प्रयत्न किया हो अथवा नहीं। जो कुछ भी मिलना है, वह मिल कर ही रहता है।
साधक-जिज्ञासुओं को भले और बुरे, सुख और दुःख, प्रेम और घृणा इत्यादि जैसे सभी द्वन्द्वों से मानसिक विरक्ति विकसित करनी चाहिए। ऐसा मानसिक समता का भाव सद्ग्रन्थों के स्वाध्याय से तथा सन्तों के संग इत्यादि से आत्म-विचार को प्राप्त करके किया जा सकता है। साधक में आत्म त्याग, आत्म-तुष्टि और आत्म-अस्वीकृति का होना आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए अति आवश्यक है।
यदि साधक अपने प्राप्त भाग्य के प्रति सन्तुष्ट रहता है और जिन इच्छाओं के प्रति पहले विचार करके आनन्दित होता था, उनके आगे भी मानसिक रूप से झुकता नहीं है, तो यह पराजित मानसिकता का द्योतक नहीं है। निश्चित रूप से यह लोमड़ी के 'अंगूर खट्टे हैं' वाली प्रवृत्ति नहीं है। स्वैच्छिक आत्म-अस्वीकृति तथा त्याग के द्वारा अथवा कुछ अनचाहा हो जाने पर भी समता बनाये रखने से अत्यधिक इच्छा-शक्ति विकसित हो सकती है; अतः यह अनिवार्य है कि चेतना की समस्त अवस्थाओं में मन का सन्तुलन बनाये रखा जाये।
३९
तकनीकी अर्थों में नाड़ी-शुद्धि क्या है? यह कैसे ज्ञात हो कि व्यक्ति ने पूरी तरह से नाड़ी-शुद्धि की अवस्था प्राप्त कर ली है?
नाड़ी-शुद्धि से अर्थ है-नाड़ियों की स्वच्छता अथवा शुद्धता। वास्तव में अँगरेजी का 'नर्व' शब्द नाड़ी का पूर्ण अर्थ नहीं है। देखा जाये तो अँगरेजी में इसके लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है।
पूर्ण उपवास (अच्छा हो यदि कुछ भी ठोस या तरल भोजन न लिया जाये), आसन-प्राणायाम का अभ्यास तथा कठोर शारीरिक व्यायाम-ये सब मिल कर नाड़ियों में से चर्बी तथा अन्य अवांछित पदार्थ निकाल कर समस्त प्रणाली में सुधार ला कर नाड़ी-शुद्धि में सहायता करते हैं। आसन एवं प्राणायाम तन्त्रिकाओं को शुद्ध कर सकते हैं, व्यदि इन्हें सही ढंग से किया जाये।
जब व्यक्ति नाड़ी-शुद्धि की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो शरीर हल्का हो जाता है। मल की मात्रा कम हो जाती है। शरीर की गति में लचीलापन और व्यवहार में सक्रियता आ जाते हैं। सुस्ती अथवा आलस्य का चिह्न भी शेष नहीं रहता। चलते समय प्रतीत होता है मानो शरीर हवा में तैर रहा हो। वाणी की कर्कशता अथवा रूखापन हट जाता है तथा सुमधुरता उसका स्थान ले लेती है। कूदना, छलाँगें जैसे लगाना और नृत्य करते हुए प्रतीत होना नाड़ी-शुद्धि प्राप्त व्यक्ति कार्य करते समय ऐसा देखा जा सकता है। व्यक्ति यो अमुक कार्य करने, अमुक लक्ष्य प्राप्त करने इत्यादि जैसी भावना के लिए अन्दर से कोई अवर्णनीय शक्ति प्रेरित करती रहती प्रतीत होती है।
४०
बिना हमारी किसी गलती के ही हमारे साथ होने वाले गलत काम या व्यवहार के लिए प्रतिशोध लेने के सबसे बढ़िया और सबसे खराब ढंग क्या हैं?
गलत व्यवहार किसी कारण से हो, अथवा निराधार हो, यदि व्यक्ति वास्तविक नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करना चाहता है और प्रभु की कृपा प्राप्त करता चाहता है, तो उसे किसी भी ढंग से प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। मन की शान्ति और सन्तुलन को किंचित् भी खोये बिना उसको शान्ति से सहन कर लें। अपने को हानि पहुँचाने वाले का भला करें। अपने को अपशब्द कहने वाले को आशीर्वाद दें। आपको जो व्यक्ति परेशान करता हो, उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। जयदेव, शम्स तबोज, ईसामसीह, गौरांग तथा अन्य सन्तों के चरित पढ़ें। भगवान् के भक्त यदि स्वयं को भगवान् के प्रति पूर्णतया समर्पित कर देते हैं, गजेन्द्र और द्रौपदी की भाँति पूर्णरूपेण भगवान् की शरण में चले जाते हैं, तो भगवान् स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रतिकार के रूप में किसी भी प्रकार का सहारा ले कर स्वयं को निम्न कोटिकृत न को। चिन्तन में भी प्रतिशोध का विचार, भले ही अपने निम्न मन की तुष्टि के लिए ही हो, व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप में दूषित कर देता है।
अपने विरोधी को भगवद्गीता अथवा रामायण जैसी आध्यात्मिक पुस्तक भेंट करना तथा अज्ञानवश अनुचित कार्य से बचने एवं आत्मज्ञान प्राप्त करने की उसके लिए प्रार्थना करना, यह सर्वोत्तम ढंग है उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने का, जिसने अकारण ही आपके प्रति अनुचित कार्य या व्यवहार किया है। भगवान् से हार्दिक प्रार्थना करते हुए मौन का पालन करें और समभाव बनाये रखें।
४१
यदि किसी उन्नत योगी को कोई गम्भीर रोग हो जाये तो क्या उसका मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है ? ऐसी परिस्थिति में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है?
नहीं, कभी नहीं! यदि देह सम्बन्धी अथवा शारीरिक कष्ट सम्बन्धी कोई विचार भी उसे आता है, या कुछ भी ऐसा होने से जो देह-मन के लिए सहन करना कठिन हो, उसे शान्ति से सह नहीं पाता, तो याद रखें, वह उन्नत योगी अथवा सन्त या संन्यासी नहीं है। वह व्यक्ति, जिसे अपने या अपने आस-पास के अथवा संसार के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं आते, वह-जो निज आत्मा में अथवा अपने प्रियतम इष्टदेव में, या अपने दयालु गुरु में ही ध्यानस्थ रहता है, और जो किसी भी प्रकार की सीमित वस्तु-परिस्थिति एवं व्यक्ति के प्रति पूर्णतया विस्मरणीय रहते हुए स्वयं का सम्बन्ध उस असीम, निरामय, अप्रतिबन्ध, सर्वव्यापक ब्रह्म से ही बनाये रखता है, वही वास्तविक एवं उन्नत योगी अथवा भक्त या ज्ञानी है, अन्य दूसरा नहीं।
अपने रोग के प्रति अथवा सीमित, नश्वर शरीर सम्बन्धी या समस्त संसार सम्बन्धी उसके उपेक्षापूर्ण भाव की समानता सारे संसार में किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। वह सदैव निज आत्म-स्वरूप में स्थित रहता है तथा किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपना सन्तुलन बिगड़ने नहीं देता। वह इस बात में दृढ़ विश्वास रखता है कि मृत्यु प्रत्येक की प्रतीक्षा में है और वह किसी-न-किसी समय आ कर प्राण हर लेगी; तथा यह भी कि शोक, मोह, क्षुधा, पिपासा, जरा और मृत्यु नामक षड् उर्मियाँ प्राणी मात्र में समान हैं, केवल मानव में ही नहीं। और यह भी कि आत्मा अमरणशील, अनश्वर और शाश्वत ब्रह्म ही है। अतः कठिन से कठिन परीक्षा की घड़ियों में भी वह मन से अशान्त अथवा विकल नहीं होता।
४२
क्या श्रीमद्भगवद्गीता सचमुच ही युद्धभूमि में भगवान् श्री कृष्ण के मुख से उच्चरित की गयी थी अथवा यह कवि की काल्पनिक गाथा है?
हाँ! इसमें किंचित् भी सन्देह नहीं है। यह सचमुच युद्धभूमि में भगवान् श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। यह केवल चिरंजीवी व्यास जी की काल्पनिक कृति मात्र नहीं है। इन दो श्लोकों को देखें, जो गीतामाहात्म्य में आपको मिलेंगे :
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः ।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता ।।
भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतम्।
गीतागंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ।।
गीता मानव कृति नहीं है। बौद्धिक तर्क-वितर्क को छोड़ कर इस बात में विश्वास रखें। भगवान् श्री शंकराचार्य और रामानुज जी, जिन्होंने गीता पर भाष्य रचे हैं, को स्मरण करें। भगवान् श्री कृष्ण ने अपनी एक भक्त लीलाबाई से स्वयं कहा है कि वह स्वयं और गीता एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, एक की पूजा करने से दूसरे की पूजा हो जाती है। गीता के अठारहवें अध्याय के ६८ से ७१ तक के श्लोक ध्यान से पढ़ें, इससे आपके हृदय में पावन ग्रन्थों के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा।
४३
कृपया क्या आप कोई ऐसे प्रभावशाली ढंग एवं उपाय बतायेंगे जिनके द्वारा काम-शक्ति रूपान्तरित हो सके तथा उसका ओज में उदात्तीकरण हो जाये ?
काया-वाचा-मनसा कठोर संयम का पालन करें, निरर्थक और व्यर्थ चिन्तन छोड़ दें। हर अवस्था एवं परिस्थिति में मन का सन्तुलन बनाये रखें और भगवान् का चिन्तन करें। शीर्षासन, सर्वांगासन तथा ऊर्ध्व पद्मासन करें, साथ ही विपरीतकरणी मुद्रा करें। सतत भगवन्नाम-स्मरण, सतत जप, ध्यान, गीता अध्ययन, भागवत तथा रामायण जैसे सद्ग्रन्थों का पाठ करते रह कर अपनी वीर्य-शक्ति की रक्षा करें। विवेक और वैराग्य (सांसारिक विषयों में आसक्ति) को विकसित करें। जैसे-जैसे वैराग्य में वृद्धि होगी, वैसे ही साथ-साथ वीर्य-शक्ति को सुरक्षित रखने के प्रयास सहज हो जायेंगे। जितना ही वीर्य सुरक्षित होगा, उतनी ही शक्ति ओज में रूपान्तरित होगी; जिसका अर्थ है-शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति का प्रचुर मात्रा में होना तथा शीघ्रतम उन्नत अवस्था को प्राप्त होना। प्राणायाम शारीरिक एवं मानसिक संयम बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। मन पर नियन्त्रण का अर्थ है-प्राण-शक्ति पर नियन्त्रण तथा वीर्य नष्ट होने पर नियन्त्रण। इस वीर्य-शक्ति पर नियन्त्रण हो जाने का अर्थ है-प्रचुर मात्रा में ओज-वृद्धि, अर्थात् आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित होने की क्षमता में वृद्धि। इच्छाओं को निम्नतम करते हुए गहन साधना करने से काम-शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जायेगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी पुस्तक 'प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य' (ब्रह्मचर्य-साधना) पढ़ें। पूछे गये प्रश्न का इस पुस्तक में विस्तृत उत्तर मिल जायेगा।
४४
क्या यदि सच न बोलना आवश्यक ही हो गया हो, अपितु अनिवार्य ही हो जाये तो सच न बोलने से समझौता किया जा सकता है? क्या ऐसे में असत्य बोलने को न्याय-संगत कहा जायेगा ?
सत्य सत्य है और असत्य तो असत्य ही है, दोनों का परस्पर उतना ही अन्तर है जितना किसी वृत्त की परिधि के विपरीत बिन्दुओं अथवा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का परस्पर अन्तर है। जो व्यक्ति नैतिक परिपूर्णता प्राप्त करना चाहता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है और धर्म से प्रेम करता है, उसे सत्य पर अटल रहना चाहिए, भले ही कितनी भी संकटपूर्ण परिस्थितियाँ हों, कैसी भी गम्भीर स्थित हो। हरिश्चन्द्र को याद करें, इतनी मुसीबतों में भी वह कैसे सत्य पर अडिग रहा। कैसे उसका नाम अभी भी उसी प्रकार चमक रहा है! हरिश्चन्द्र सत्य की साकार प्रतिमा थे। यह एकमात्र उदाहरण ही व्यक्ति को भयंकर से भयंकर स्थितियों का सामना होने पर भी सत्य पर टिके रहने की शक्ति देने में पर्याप्त है। भले ही कितना भी आवश्यक एवं अनिवार्य हो, और हालात की माँग निजी स्वार्थवश कितनी भी आवश्यक हो, झूठ को तो निष्ठुरता से दूर भगा देना चाहिए। सत्य और झूठ को कभी भी एक-दूसरे से मिलाया नहीं जा सकता। एक का दूसरे से मिलान बहुत ही गलत है। इसमें सन्देह नहीं कि भागवत तथा अन्य पुराणों में कुछेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ असत्य बोलना सही ठहराया गया है; किन्तु ऐसी घटनाएँ अपवाद स्वरूप ही हैं, वह हर समय और हर व्यक्ति के लिए सही नहीं मानी जा सकतीं। इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक 'ऐथिकल टीचिंग्स' (नैतिक शिक्षा) पढ़ें।
४५
किसी व्यक्ति को यदि प्रारब्धवश युवावस्था में ही मृत्यु अथवा गम्भीर रोग से ग्रस्त होना लिखा हो, तो क्या महामृत्युंजय मन्त्र उसे इन पर विजय पाने में सहायता कर सकता है?
परमात्मा की कृपा से प्रारब्ध को पराजित किया जा सकता है। भगवान् की कृपा वहाँ होती है जहाँ सच्ची भक्ति और पूर्ण पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तभी सम्भव है, जब मन पचित्र हो। मन तब पवित्र होता है, जब व्यक्ति दया और दान करता हो। जब भगवान् कृपा एवं करुणा बरसाते हैं, तो दैवी नियम उसके आगे नहीं चलते। उनकी कृपा में अपार शक्ति है। हम मार्कण्डेय का उदाहरण जानते हैं जिसने अपने पुरुषार्थ तथा भगवद्-भक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उसके प्रारब्ध में युवावस्था में मृत्यु निश्चित थी; किन्तु जब भगवान् की कृपा हुई तो यमराज अपनी इच्छा पूर्ति कर नहीं सके। अतः तीव्र पुरुषार्थ से प्रारब्ध को पराजित करना सम्भव है।
४६
कुछ दार्शनिक तर्क एवं बुद्धि पर आधारित जीवन के ऊपर बहुत बल देते हैं। आपका क्या विचार है?
तर्क और बुद्धि को सर्वोच्च स्थान कैसे दिया जा सकता है? मदोन्मत्तता की स्थिति में मन, बुद्धि और तर्क-शक्ति व्यर्थ हो जाते हैं। ऐनिस्थीसिया (संज्ञाहीनक औषधि) के प्रभाव से तार्किक मन कहाँ रहता है? पन्द्रह दिन तक निरन्तर पूर्ण उपवास के बाद क्या व्यक्ति की तार्किक बुद्धि पूर्णतया सही रहती है? निद्रा और मूर्छा की अवस्था में यह लुप्त हो जाती है। ऐसी जड़ी-बूटियाँ भी हैं जो खाते ही मन को पंगु बना देती हैं। अतः ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे व्यक्ति की तार्किक बुद्धि असमर्थ हो कर कार्य करना बन्द कर देती है। इस तर्कशील मन को अथवा तर्क पर आधारित जीवन को सर्वोच्च स्थान कैसे दिया जा सकता है? अन्तर्ज्ञान ही सर्वोच्च क्षमता है और जब व्यक्ति इस मनः शक्ति को पूर्ण विकसित कर लेता है, तब उसका विकास परिपूर्ण रूप से होता है तथा वह आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। समाधि की अवस्था में प्राप्त हुआ ज्ञान ही उच्चतम ज्ञान है। यही सम्यक्-दृष्टि अथवा तत्त्वज्ञान है।
४७
समस्त औषध-पद्धतियों में से कौन-सी पद्धति सबसे अधिक प्रभावशाली और अहानिकर है? कृपया कारण सहित बतायें।
सभी चिकित्सा पद्धतियों के अपने-अपने लाभ और हानियाँ हैं। प्रत्येक की दूसरियों पर प्राधान्यता है। प्रत्येक की अपनी कमियाँ हैं। मेरे दृष्टिकोण से आयुर्वेद का मेरे हृदय में सर्वोच्च स्थान है। इसका धन्वन्तरि भगवान् द्वारा प्रतिपादन किया गया है, जो कि आयुर्वेद के पिता हैं। आधुनिक समय में जितने चिकित्सा विज्ञान हैं, उनमें आयुर्वेद का स्थान सर्वोपरि है। इसका प्रभाव स्थायी और अबाधित है। अन्य अधिकांश चिकित्सा शास्त्रों का यह मूल एवं स्रोत है। जहाँ तक बिना देरी के तत्काल उपचार का प्रश्न है ऐलोपैथी (विषम चिकित्सा) का स्थान सबसे आगे और सबसे ऊपर है। होमियोपैथी सबसे अधिक हानि रहित पद्धति है और मूल्य की दृष्टि से भी सबसे सस्ती है।
४८
मैं जप, ध्यान इत्यादि की साधना का अभ्यास करता रहा हूँ; किन्तु मेरा मन एकाग्र नहीं हुआ, इधर-उधर जाता रहा। मैं इसे नियन्त्रित करने का प्रयत्न भी करता रहा, किन्तु सन्तोषजनक सफलता नहीं मिली। जितनी उन्नति मेरी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो रही है। क्या करूँ ?
यदि आप शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं तो आपको और अधिक प्रयास करना चाहिए था। और अधिक जप, धारणा और ध्यान करें। वैराग्य और अभ्यास को बढ़ायें। रात्रि के समय सत्संग और कीर्तन करें। निराश न हों; समय आने पर आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। धीरे-धीरे लगे रहें।
४९
कहते हैं कि यह तो, एक अकेले की एक की ओर उड़ान है। फिर गुरु की अथवा गुरु-कृपा की कहाँ आवश्यकता रह जाती है? उपनिषदों में भी कहा गया है कि ईश-कृपा से ही सब-कुछ होगा।
ईश-कृपा आप कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप स्वयं का शुद्धिकरण कर लेंगे। स्वयं को अनुशासित कैसे करना है, यह आप कैसे जानेंगे? उनको ध्यानपूर्वक देख कर जो पहले परिपूर्णता-प्राप्ति के इस पथ पर चल कर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, वह कौन हैं? यही हैं, जिन्हें गुरु कहा जाता है। अतः आपको उनसे सहायता लेने की आवश्यकता है। उनके निजी व्यक्तिगत उदाहरण की, उनसे उत्साह और उनकी कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुरु और उनकी कृपा, दोनों ही आवश्यक हैं। यह सभी कुछ अनिवार्य है- आत्म-कृपा, गुरु-कृपा और ईश्वर-कृपा।
५०
क्या अधिक बड़ा है-प्रेम या बुद्धि, भक्ति या ज्ञान ?
अपनी बुद्धि को डिब्बे में बन्द रहने दें! प्रेम और विवेक एक ही हैं। भक्ति और जार एक हैं। प्रेम ज्ञान की ओर ले जाता है। एक, दूसरे की सहायता करता है। लोग पुस्तके एद लेते हैं और तर्क करना आरम्भ कर देते हैं, यह बड़ा है या वह बड़ा है? यह सब पूर्वता है। भगवान् प्रेम और ज्ञान, दोनों ही हैं। व्यक्ति को इन निरर्थक बातों में समय नष्ट नही करना चाहिए।
५१
स्वामी जी ! मैं लखनऊ में रहता हूँ। यह ऋषिकेश से बहुत भिन्न है। जब मैं ऋषिकेश से लखनऊ वापस जाऊँगा, तो यहाँ के शान्त वातावरण की कमी बहुत अधिक लगेगी। वहाँ का वातावरण अत्यन्त बनावटी है। मैं वहाँ क्या साधना करूँ ?
क्यों? आप वहाँ भी बहुत बढ़िया साधना कर सकते हैं। संसार बाधा नहीं है। आपको वेदान्त का अत्यन्त विस्तृत एवं व्यावहारिक ज्ञान है। रामतीर्थ जी की ज्वतन्त आत्मा आप में हैं। ब्राह्ममुहूर्त ध्यान कक्षाएँ आरम्भ कर दें। लखनऊ निवासियों की इन रूप में आप महान् सेवा कर सकते हैं। मोहल्ले-मोहल्ले जा कर वेदान्त पर प्रवचन को। प्रत्येक मोहल्ले में स्वाध्याय केन्द्र खोलें। क्रम से प्रत्येक मोहल्ले में प्रातः ब्राह्ममुहूर्त में ध्यान-कक्षाएँ चलायें। इससे आप समस्त मानव जाति की और स्वयं अपनी सेवा करेंगे। लोगों को उनके जीवन के वास्तविक लक्ष्य के प्रति जागरूक करें। ऐसा करने से आपकी आत्मा भी जागरूक रहेगी।
५२
क्या यह सम्भव है कि कोई जीवात्मा, जो इस जन्म में पुरुष शरीर में जन्मी है, उसका आगामी जन्म स्त्री शरीर में हो ?
हाँ, हो सकता है। विभिन्न शरीर धारण करते हुए जीवात्मा को विविध अनुभवों में से निकलना पड़ता है। पुरुष शरीर में जीवात्मा में निर्भीकता, बल इत्यादि गुणों तथा नारी देह में धैर्य, दया, क्षमा इत्यादि गुणों का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त न तो कोई पुरुषदेहधारी पूर्णतया पुरुष के गुण लिये होता है और न कोई स्त्री पूरी तरह से नारी गुणों से सम्पन्न होती है। पुरुष देह में नारी और नारी देह में पुरुष भी होते हैं। मनुष्य में पशुओं के लक्षण भी पाये जाते हैं। कुछ पुरुषों में कुत्ते के, किसी में गधे के, किसी-किसी में गीदड़ के और किसी में शेर के भी स्वाभाविक लक्षण होते हैं। एक जन्म में जैसा भी गुण मुख्य रूप से विकसित हो जाता है, आगामी जन्म में जीवात्मा वैसी ही देह धारण कर लेती है। इसलिए दिव्य गुणों को विकसित करें। आप शीघ्र उन्नत होंगे और अन्ततः दिव्यता का ही रूप धारण कर लेंगे।
५३
पुनर्जन्म के सम्बन्ध में निष्कर्षतः आपके क्या विचार हैं? क्या आप सचमुच पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं?
क्या कहा ? हिन्दू परिवार में जन्म ले कर, अपनी शिराओं में महान् ऋषियों का रक्त प्रवाहित होता होने पर भी क्या आपके मन में इसके प्रति कोई सन्देह हैं? हाँ, निःसन्देह पुनर्जन्म होता है।
सर्वप्रथम, ऐसे सैकड़ों चमत्कारिक एवं अद्भुत उदाहरण छोटे-छोटे लड़के-लड़कियों के देखने में आये हैं, जहाँ उनमें अचानक अत्यधिक ज्ञान का उदय हो जाता है। एक बालिका, जिसने कभी कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी, गीता-पाठ करती है। इसका आप इसके अतिरिक्त, कि उसने अपने गत जन्म में गीता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अब परमात्मा की कृपा से वह ज्ञान इस जन्म में भी उसके चेतन मन में आ गया है, अन्य क्या स्पष्टीकरण आप दे सकते हैं? और फिर, आत्मा की उन्नति अथवा विकास के लिए पुनर्जन्म एक आवश्यकता है। परिपूर्णता को एक ही जन्म में प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछेक मूल-सद्गुण विकसित करने के लिए भी अनेकों जन्म लग सकते हैं। और यदि आपने आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करना हो तो सभी सद्गुणों में परिपूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है। आपको पूर्ण रूप से आत्म-शुद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। अतः जीवात्मा के पूर्णरूपेण विकसन के लिए पुनर्जन्म आवश्यक है।
आपने कभी किसी कीट को वृक्ष के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाते हुए देखा है? यह एक पत्ते के अन्तिम छोर तक पहुँच कर, जब दूसरे पत्ते को पकड़ लेता है, केवल तभी पहले पत्ते को पूरा छोड़ता है। जीव की यात्रा भी इसी प्रकार से है। एक शरीर को छोड़ने से पहले ही यह अपने कर्मानुसार एवं इच्छाओं के अनुसार दूसरी देह (स्थूल या सूक्ष्म) का निर्माण कर लेता है; और यह अपने समस्त संस्कारों एवं वासनाओं सहित नये शरीर में प्रवेश कर जाता है।
५४
मृत्यु और आगामी जीवन के बीच का अन्तराल कितना होता है? इस बीच के समय में जीवात्मा कहाँ रहती है ?
यह अन्तराल सबका अलग-अलग होता है। यह दो वर्ष का भी हो सकता है, और २०० वर्षों का या इससे अधिक समय का भी हो सकता है। कोई निश्चित नियम इसके सम्बन्ध में नहीं है। यदि इस संसार में आसक्ति बहुत अधिक हो, तो मृत्यु के तुरन्त बाद ही जीवात्मा पुनः जन्म ले सकता है। देहरादून में एक लड़की है जिसे अपने पिछले जन्म की पूरी स्मृति है। गत जन्म के चार वर्षों बाद उसने पुनः यह जन्म ले लिया। जिन्होंने अपने जीवन-काल में बहुत से भले कार्य किये हैं, वे इस धरती पर पुन: आने से पहले २०० या ३०० वर्ष की अवधि तक स्वर्गलोक में रहते हैं।
दुष्ट व्यक्ति अन्य दूसरे स्थान में जाता है। आप इसे नरक कह सकते हैं, अथवा यह ऐसा स्थान हो सकता है, जहाँ उसे अपने इच्छानुकूल सुख-भोग प्राप्त नहीं होते। मद्यपान करने वाले को वहाँ मदिरा नहीं मिलती। यह जेल के समान स्थान भी हो सकता है, जहाँ उसे चट्टानें तोड़ने का अथवा ऐसा ही कोई अन्य कठोर काम करना पड़ सकता है। किन्तु जिस व्यक्ति ने भले काम किये होते हैं अथवा जो लोकोपकारक होता है और उसने लोगों के लिए कुएँ खुदवाने, धर्मार्थ चिकित्सालय बनाने जैसे सेवा कार्य किये होते हैं, वह व्यक्ति स्वर्गलोक में जा कर दीर्घ काल तक सुख भोगेगा।
५५
यदि आत्मा अमर है, तो स्वामी जी, आप अपना जन्म-दिन-जो कि शरीर से सम्बन्धित है-क्यों मनाते हैं?
मैं अपना जन्म-दिन नहीं मनाता, भक्त मनाते हैं। ऐसे जन्म-दिवसों को मनाना परब्रह्म की पूजा करने के समान है। गुरु की पूजा परब्रह्म की पूजा है। भक्तजनों को जन्म-दिन मनाने से आनन्द प्राप्त होता है, और वे लाभान्वित होते हैं, उन्नत होते हैं। जब जन्म-दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष उस दिन से पुनः एक आध्यात्मिक तरंग उत्पन्न हो जाती है तथा अधिक-से-अधिक लोगों को 'द डिवाइन लाइफ सोसायटी' के और मेरी शिक्षाओं के सम्बन्ध में जानने का अवसर प्राप्त होता है। जन्म-दिवस महोत्सव समस्त साधकों को जीवन का वास्तविक लक्ष्य स्मरण कराने के लिए अनुस्मारक होता है। ऐसे अवसरों पर व्याप्त होने वाला भक्तों का पावन और ग्रहणशील भाव उन पर गुरु और भगवान् की कृपा-वृष्टि करता है। जन्म-दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए असंख्य भक्तों के हृदयों में उत्पन्न हो कर सर्वत्र व्याप्त होने वाली शान्ति और भक्ति इत्यादि की भावनाएँ धरा पर दूर-दूर तक पहुँच कर शान्ति, सामंजस्य और आध्यात्मिकता का विकास करती हैं।
हिन्दू जो बुद्ध जयन्ती, महावीर जयन्ती इत्यादि के रूप में धार्मिक गुरुओं और सन्त-महात्माओं के जन्मोत्सव मनाते हैं, वह निरर्थक नहीं हैं। हिन्दू पंचांग में ऐसी बहुत-सी जयन्तियों के तथा अन्य पावन दिनों के सम्बन्ध में अंकित है, जिससे कि ये सब जयन्तियाँ और पावन दिवस लोगों को, उनके लिए आवश्यक आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करें और वे जीवन के परम लक्ष्य-आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए विकसित उत्साह के साथ लग जायें। जितने अधिक ऐसे पावन दिवस मनाये जाते हैं, उतना ही अधिक हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति की साधना में वृद्धि करने की प्रेरणा के अवसर मिलते हैं।
५६
जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ, तो निम्न मन इधर-उधर भटकता रहता है, किन्तु दूसरा मन बिना रुके स्तोत्र पाठ करता जाता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव बन चुका है। परन्तु जब मैं पूरा सचेत हो कर श्लोक उच्चारण करने का प्रयास करता हूँ तो कभी-कभी भूल जाता हूँ और कई बार तो मुझे स्तोत्र आरम्भ से दोहराना पड़ता है। तो क्या मन दो हैं? इस कठिनाई से छुटकारा कैसे हो ?
नहीं। मन दो नहीं हैं। किन्तु मन की एकाग्रता धीरे-धीरे बढ़ती है, और मन का वह भाग जो आध्यात्मिकता की ओर रुचि रखता है-आप इसे उच्चतर मन कह सकते हैं-वह स्वयमेव साधना में प्रवृत्त हो जाता है, जब कि इसका दूसरा भाग, जो सांसारिक संस्कारों के प्रति अधिक झुकाव रखता है, वह उन्हीं संस्कारों में उलझा रहता है। स्वभाव की शक्ति यन्त्रवत् प्रार्थनाएँ दोहराती रहती है। किन्तु आपको चाहिए कि उच्चतर भाग को श्लोक के अर्थों पर एकाग्र करके रखें। जब मन की एकाग्रता स्थिर रहेगी तो निम्न मन को विषय से भटकने का अवसर कम मिलेगा। लापरवाही से की जाने वाली साधना की सारी समस्या यह रहती है कि यह यन्त्रवत् अर्थात् मशीन के समान चलती रहती है और साधक के जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ पाती।
५७
क्या हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों में ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो पूर्ण हुई हों ? यदि हैं, तो कृपया उनके सम्बन्ध में बतायें।
भगवान् ने हमें सदा के लिए एक वचन दे रखा है कि जब भी कभी धर्म की हानि होगी अर्थात् धर्म पर संकट आ पड़ेगा और जब अधर्म, धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा तो वह धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरा पर अवतरित होंगे। उस वचन को पूरा करने के लिए वे समय-समय पर अनेकों बार ऐसे सन्त-महात्माओं के रूप में आते रहे हैं जिहोंने बाह्य आक्रमणों से धर्म की रक्षा की है और धर्म को नष्ट होने से बचाया है। उन्होंने हिन्दू-धर्म में नयी शक्ति और नूतन उत्साह का संचार किया है। इसीलिए हिन्दू-धर्म निरन्तर समृद्ध हो रहा है। जब भी आवश्यकता होगी, सन्त-महात्मा आ जायेंगे, कहीं आकाश से नहीं, प्रत्युत् यहाँ के लोगों में से ही आयेंगे।
हिन्दू-धर्म पूर्णरूपेण केवल एक ही सन्त अथवा धर्मदूत में विश्वास नहीं रखता। पुराणों में भविष्य में होने वाली परिस्थितियों के सम्बन्ध में की गयी भविष्यवाणियाँ भी सत्य सिद्ध हुई हैं।
५८
यदि मैं ईसामसीह से प्रेम करता हूँ, तो क्या मुझे केवल अकेले उनसे ही प्रेम करना चाहिए; अन्य दिव्यात्माओं, यथा मदर मेरी और अन्य प्रतीकों अथवा मूर्तियों से नहीं करना चाहिए?
नहीं। एकमात्र यीशु के प्रति ही प्रेम नहीं होना चाहिए, भले ही अन्य ईसाई सन्त उन जैसे महान् न भी हों। यदि आपमें उनके प्रति भी श्रद्धा है तो उन्हें यीशु की उसी दिव्यता का प्रकटीकरण मानते हुए, उनकी भी पूजा की जा सकती है। भगवान् के सभी 'सन्देशवाहक' (सन्त) हमारी श्रद्धा और भक्ति के एक-समान पात्र हैं। किसी के स्वभाव और भावनाओं के अनुसार कोई अधिक श्रद्धा का पात्र हो सकता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति दूसरों का बहिष्कार कर दे। एकमात्र कोई भी एक सन्त या धर्मदूत भगवान् का आदेश-पत्र ले कर अथवा स्वर्ग-द्वार की चाबी ले कर नहीं आया है।
५९
मेरा दृढ़ मत है कि संतों से प्रार्थना करना अथवा उनकी पूजा करना पूर्णतया गलत है। उन्होंने भगवान् से प्रार्थना की और स्वयं अपने लिए मोक्ष प्राप्त किया, उसी तरह हम भी किसी सन्त-महात्मा पर निर्भर किये बिना अपने लिए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है। सन्त और महात्मा हमारी श्रद्धा और भक्ति के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ईश्वर-साक्षात्कार का मार्ग दर्शाया है। एक नौसिखिया, जो अभी-अभी ही नौकरी में प्रविष्ट हुआ है, उससे यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह अपने उस वरिष्ठ व्यक्ति के प्रति विनम्रता एवं ग्रहणशीलता का भाव रखे, जो उसे प्रशिक्षित कर रहा है, भले ही वह प्रशिक्षक भी उसी जैसा एक व्यक्ति है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। सन्तों को सम्मान देने से तथा उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आप भगवान् को अधिक भली-भाँति जान सकेंगे और प्रेम कर सकेंगे।
६०
कोई व्यक्ति मुझे यह बताने का प्रयास कर रहा है कि (उसके शब्दों में) 'निर्विकल्प समाधि केवल एक ऐसी स्नायु-दशा है जिसके साथ-साथ कतिपय मनःशक्तियों को शक्तिहीन कर दिया जाता है।' मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? क्या इसका कोई उत्तर है?
जो मनुष्य निर्विकल्प समाधि की वैधता को समझ नहीं सकता, उसे समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है। तार्किक बुद्धि ने भले ही पर्याप्त उन्नति कर ली हो, किन्तु संशयवादी व्यक्ति को इस सत्य के प्रति जागरूक होने के लिए और अधिक उन्नत होना पड़ेगा। ऐसे संशयवादियों को उत्तर देने का प्रयत्न करने से पहले व्यक्ति को दार्शनिक निहितार्थों एवं अनुभूति के रहस्यात्मक अर्थों का भली-भाँति अध्ययन किया हुआ होना चाहिए।
६१
'दी लाइफ डिवाइन' की एक अत्यन्त दुरुह तर्कशास्त्र से सम्बन्धित श्रृंखला में अन्ततः श्री अरविन्द महर्षि ने यह कहते हुए परिसमाप्ति की, "और ये सब व्याख्याएँ कुछ भी व्याख्या नहीं करती हैं।" तब फिर क्या सचमुच कोई लाभ है, कोई अर्थ है कि इस शब्द-जाल की बारीकियों में जाया जाये और इनका अनुसरण किया जाये ?
अन्तिम अर्थों में, शब्द सत्य की व्याख्या नहीं करते; किन्तु वह संकेत देते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सत्य की सीधी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। शब्दों का सापेक्ष मूल्य है और उनको निश्चित रूप से उपयोग में लाना चाहिए, भले ही वह हमारे वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति नहीं करते। सत्य के ज्ञान से सम्बन्धित बाधाओं को सापेक्ष साधनों द्वारा दूर किया जा सकता है और इस प्रकार परम सत्य का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है।
६२
मुझे तो ऐसे लगता है कि किसी भी पूर्णतया विकसित योगी ने कभी भी केवल उच्च, गूढ़, अव्यावहारिक अथवा अन्तर्दर्शी विषयों पर लिखने और थोड़ी सी रुचि रखने वाले लोगों को प्रभावित करने के अतिरिक्त संसार से सम्बन्धित अथवा विकास से सम्बन्धित कुछ भी योगदान नहीं किया।
तब फिर आप, अत्यधिक महान् एवं सर्वोत्कृष्ट प्रतीत होने वाली अरविन्द महर्षि की पुस्तक 'दी लाइफ डिवाइन' जिसे लगभग कोई भी पढ़ता नहीं, और कोई भी समझ नहीं सकता, अथवा 'ट्रिटाइज़ ऑन कॉमिक्स फायर' पुस्तक या तो आपकी पुस्तकें, जिनमें से प्रायः सभी ऐसी लगती हैं जो किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से सांसारिक दृष्टि से सहायता नहीं पहुँचातीं, इन सबके सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं?
यह सोचना ठीक नहीं है कि योगी जन केवल लिखते भर ही हैं, वे मानवता की उन्नति के लिए कभी कुछ नहीं करते। जो सहायता वे करते हैं, उसे साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता, और मनुष्य को योगियों से किसी विशेष प्रकार की सहायता की आशा रखने का अधिकार भी नहीं है; क्योंकि योगी वही करते हैं जो वास्तव में अच्छा है, वह नहीं जो मनुष्य को भौतिक दृष्टि से सुविधाजनक है। अतीन्द्रिय अथवा अतिभौतिक विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें, जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के ढंग की भली-भाँति व्याख्या करती हैं, वह संघर्षरत मानवता के लिए अत्यन्त सहायक हैं। योगी जन ऐसी पुस्तकें दूसरों के भले के लिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी लिखते हैं। किन्तु वे इससे अधिक भी बहुत कुछ करते हैं, वे सीधी एवं अदृश्य सहायता पहुँचा देते हैं।
६३
'केवल कुम्भक' कैसे किया जाता है? इसका अभ्यास करना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। इसे 'पूरक और रेचक से रहित कुम्भक' कहा गया है। यह समझ नहीं आता; क्योंकि कुम्भक से पहले श्वास को लेना अथवा छोड़ना तो आवश्यक है।
'केवल कुम्भक' के अभ्यास के सम्बन्ध में आपकी उलझन आश्चर्यजनक नहीं है; क्योंकि पूरक या रेचक किये बिना कुम्भक करना असम्भव लगता है। किन्तु इसका अर्थ यह है कि केवल कुम्भक में श्वास को-अचानक ही किसी भी क्षण, जब मन एकाग्र होने ही वाला होता है तब-अवरुद्ध कर लिया जाता है।
किसी ऐसी विशिष्ट मानसिक स्थिति के क्षण प्राण का विराम, योगी के लिए ऐसे समय में जब कि उसका मन धारणा के लिए लगभग तैयार ही होता है, अत्यन्त सहायक हो जाता है। अतः 'केवल कुम्भक' धारणा के लिए अनमोल सहायता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस कुम्भक की प्रक्रिया में पूरक अथवा रेचक की ओर स्वैच्छिक ध्यान नहीं दिया जाता। इसे हम 'श्वास को अचानक अवरुद्ध' करना कह सकते हैं। योगी सुविचारित पूरक अथवा रेचक, 'केवल कुम्भक' से पूर्व नहीं करता है। जब उसने 'केवल कुम्भक' में जाना होता है तो उस समय श्वास-प्रश्वास की जो भी स्थिति हो, उसकी ओर ध्यान न देता हुआ 'केवल कुम्भक' में चला जाता है। यह उस समय पूरक के मध्य में अथवा रेचक के मध्य में कहीं भी हो सकता है। श्वास आधा अन्दर अथवा आधा बाहर भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि श्वास पूरा लिया जा चुका हो अथवा पूरा छोड़ दिया गया हो। श्वास की चाहे जो भी स्थिति हो, जैसे ही एकाग्रता होने लगती है, उसी समय ध्याता, 'केवल कुम्भक' में तत्काल श्वास को रोक देता है। मुझे विश्वास है कि अब आप भली-भाँति समझ गये होंगे।
६४
योग के ज्ञान का प्रचार करने के मेरे कार्य में आप मुझे कोई विशेष परामर्श देंगे ?
व्यावहारिक योगाभ्यास सम्बन्धी निर्देशन देने के साथ-साथ सदैव सदाचार, यम और नियमों के महत्त्व पर पर्याप्त बल दें। विद्यार्थियों को उदात्त आदर्शवाद की प्रेरणा दें। उनको उदात्त सद्गुण अपनाने, भलाई करने और निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहें। आपको उनके लिए निश्चित रूप से आत्म-शुद्धि और स्व-नियन्त्रण की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। मनुष्य की मूलभूत प्रकृति में रूपान्तरण लाना ही वास्तविक आन्तरिक योग है। मानव को, सम्पूर्णतया आध्यात्मीकरण करने की प्रक्रिया के द्वारा उसके निम्नतर स्वभाव का स्थान धीरे-धीरे उज्ज्वल दिव्य स्वभाव को ले लेना चाहिए। यह सब अत्यन्त प्रभावपूर्ण ढंग से, किन्तु साथ ही अत्यन्त सहानुभूति, समझदारी एवं सूक्ष्म दृष्टि से करना चाहिए। उद्देश्य तो दिव्य चेतना प्राप्त करना है।
६५
जब चिकित्सक भी असफल हो जाते हैं, तब क्या प्रार्थना रोगों को दूर कर सकती है? क्या यह सत्य है कि प्रार्थनाओं द्वारा ऐसी बहुत-सी बातें हो सकती हैं जिनको यह संसार स्वप्न में भी नहीं सोच सकता ?
चिकित्सक तथा औषधियाँ केवल भगवान् के हाथ के उपकरण हैं। जब तक भगवान् न चाहें कोई भी व्यक्ति रोगी का उपचार नहीं कर सकता, और कोई भी रोग-मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य को परिश्रमपूर्वक और धैर्यपूर्वक अपनी ओर से हर सम्भव प्रयास करना चाहिए, किन्तु प्रत्येक परिणाम के लिए परमात्मा की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। कष्ट को शान्तिपूर्वक सहन करना और उसे भगवान् का भेजा हुआ वरदान मान लेना, ज्ञान है। प्रार्थना व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों को जागृत कर देती है। यह भगवान् द्वारा प्रवाहित होने वाली शक्तियाँ ही हैं जो निश्चित रूप से चमत्कार कर सकती हैं।
६६
आपने कहा है कि निवृत्ति-मार्ग के साधकों को या तो बैंक में थोड़ा-बहुत धन रखना चाहिए, नहीं तो उसे भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहना चाहिए। अब मेरे पास न तो धन है और न ही मुझे भिक्षा के लिए हर दरवाजे पर जाना अच्छा लगता है; किन्तु मुझे संन्यास लेने की तीव्र इच्छा है। क्या आप मेरी यह पिपासा शान्त करने का ढंग बताने की कृपा करेंगे?
समस्त भारत में ऐसे बहुत से बढ़िया से बढ़िया आश्रम हैं, जहाँ निष्काम सेवा सहित कार्य चलते हैं। उन्हें सदा ही सच्चे और समर्थ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहती है। आप ऐसे किसी भी आश्रम में रह सकते हैं और वहाँ आश्रम की गतिविधियों में सहायता कर सकते हैं। वहाँ वे आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। किन्तु एक से दूसरे आश्रम में स्थान न बदलते रहें। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी एक का चयन कर लें और फिर वहीं पर स्थाई रूप से रहें।
६७
मैंने पढ़ा है कि किसी एक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि उस व्यक्ति को कोई बहुत अधिक अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, तो वह उस व्यक्ति का शिष्य बन सकता है; और अब भले ही वह पहले वाले व्यक्ति का शिष्य नहीं रहा है, तो भी उसे उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। आपके इस विषय में क्या विचार हैं?
संसार में अधिकांश लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि वे ब्रह्मनिष्ठ सन्तों के सम्पर्क में आ सकें। उनके साथ प्रायः ऐसा हो जाता है। बहुत से परिवारों में प्रायः कुलगुरु बनाने की परम्परा होती है और ऐसे हर परिवार का अपना-अपना कुलगुरु होता है तथा उस परिवार में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को उसी गुरु को अपना गुरु मानना पड़ता है। यह व्यक्ति शास्त्रों में बताये गये स्तरों के अनुसार किसी भी प्रकार से गुरु कहलाने के योग्य नहीं होता। यह आध्यात्मिक व्यक्तित्व-सम्पन्न भी नहीं होता, केवल एक धार्मिक व्यक्ति होता है। यह ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता; किन्तु पद खाली न रहे, इस दृष्टि से उसे धार्मिक नेता के रूप में निर्धारित कर लिया जाता है। साधक जिज्ञासु उससे दीक्षा प्राप्त करके अपना गुरु मान लेता है और उसके उपदेशानुसार साधना आरम्भ कर देता है तथा वह कुछ सीमा तक उन्नति भी कर जाता है। किन्तु यह केवल वहीं तक ही हो पाती है, जहाँ तक वह गुरु पहुँच सका होता है। उस स्तर से आगे ले जाने की क्षमता उसके गुरु में नहीं होती, क्योंकि वह ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि साधक को उच्चतर स्तर तक पहुँचे हुए गुरु का सम्पर्क प्राप्त हो जाये, तो वह निश्चित रूप से उसका शिष्य बन सकता है। वास्तव में यदि वह पहला गुरु एक सच्चा एवं निष्कपट व्यक्ति है तो वह स्वयं ही अपने उस शिष्य को अधिक उपलब्धि प्राप्त गुरु के चरणों की ओर निर्दिष्ट कर देगा।
यदि यह गुरु बदलने का प्रश्न ऐसे साधक के मन में उठता है जिसने ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त की हुई है जो उच्चतम स्थिति तक पहुँचा हुआ है, तब फिर कमी साधक में है, गुरु में नहीं। और ऐसी स्थिति में साधक यदि अन्य गुरु के पास चला भी जाये, तो भी उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। उसे निश्चित रूप से अपनी कमी दूर करनी चाहिए और एक ही गुरु के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। गुरु परिवर्तित करने की अपनी इच्छा को दृढ़तापूर्वक हटा देना चाहिए।
शास्त्र हमें बताते हैं कि यदि हमने एक बार ब्रह्मनिष्ठ सन्त को अपना गुरु मान लिया है, तो हमें अपनी निष्ठा को बदलना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक सम्बन्ध शाश्वत होता है। यदि साधक उसे तोड़ने का प्रयत्न करता है और अन्य सभी तरह के सिद्धों एवं ज्ञानियों के पीछे भागता फिरता है, तो वह अपने पथ पर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। उपनिषदों के मन्त्र में इस सम्बन्ध में अत्यन्त सुन्दर ढंग से कहा गया है :
यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।।
अर्थात् भगवान् के प्रति जिसकी परम भक्ति है और उतनी ही भक्ति अपने गुरु के प्रति है, उसके समक्ष उपनिषदों के सत्य स्वयमेव ही प्रकट हो जायेंगे। यदि भगवान् के प्रति भक्ति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो गुरु के प्रति भक्ति को भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
एकलव्य के महान् उदाहरण को न भूलें। उसने तो अपने गुरु के दर्शन तक नहीं किये थे, फिर भी उसकी भक्ति इतनी महान् थी कि उसने अपने गुरु की प्रतिमा बना कर रख ली और उसकी भावना इतनी गहन थी कि गुरु की मिट्टी की प्रतिमा ने ही उसे शर विद्या के गुप्त रहस्यों में पारंगत कर दिया। वास्तव में भाव का ही मुख्य महत्त्व है।
हाँ, उपगुरु अनेकों हो सकते हैं। भागवत में वर्णित अवधूत के आख्यान से हमें यही शिक्षा मिलती है। हमें सभी सन्तों का सम्मान करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु हममें आध्यात्मिकता का बीज बो देते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि उसे जल से सींचें, ताकि वह हमारे भीतर विकसित हो और ठीक समय पर हमें आत्म-साक्षात्कार का फल प्रदान करे।
६८
मैं अपने सोने का समय कम करना चाहता हूँ और निद्रा पर भी नियन्त्रण करना चाहता हूँ। क्या मुझे इसके लिए किसी औषधि की सहायता ले लेनी चाहिए?
औषधि की सहायता से आपको निद्रा कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे तो आपकी शरीर-व्यवस्था बिगड़ जायेगी। शरीर को निद्रा के द्वारा पर्याप्त आराम दिलाना अत्यन्त आवश्यक है। जब आप नियमित रूप से गहन समाधि में प्रवेश करने लग जाते हैं, तो शरीर-प्रणाली को स्वयमेव ही पर्याप्त आराम मिल जाता है, तब निद्रा को घटाया जा सकता है। इससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
निद्रा को अत्यन्त धीरे-धीरे तथा सावधानी से कम करना चाहिए। पहले, एक मास तक ९.३० पर सोयें और प्रातः ४ बजे उठ जायें। एक मास के बाद १० बजे सोयें और सुबह ३.३० बजे उठ जायें। फिर एक मास के बाद १०.३० बजे सो जायें और प्रातः ३ बजे उठना आरम्भ कर दें। इस प्रकार आप धीरे-धीरे अपनी नींद घटा सकते हैं। दिन के समय सोना निश्चित रूप से बन्द कर देना चाहिए।
६९
यदि भगवान् सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान् हैं, तो वह ऐसा क्यों नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना काम ठीक तरह से करे?
प्रत्येक व्यक्ति अपना काम ठीक प्रकार से ही करता है। चोर निश्चित रूप से चोरी करता है। दुष्ट व्यक्ति अवश्य ही दुष्कर्म करता है। यह कर्तव्य कर्म हैं। याद रखें, यह संसार त्रिगुणात्मक और सापेक्ष्य है। पाँव की प्रत्येक गति, प्रत्येक कदम सत्-चित्-आनन्द की ओर का ऊर्ध्वगामी प्रयास है। विश्व एक सापेक्ष्य जगत् है। वेश्याएँ, सन्त, दुर्जन, राजा और रंक सभी अपने-अपने निश्चित कामों में लगे हुए हैं। अच्छाई और बुराई सापेक्ष्य शब्दावलियाँ हैं। बुराई का अस्तित्व भलाई को महिमान्वित करने के लिए है। घृणा का अस्तित्व प्रेम को महिमान्वित करने के लिए है। एक दुष्ट व्यक्ति सदैव दुष्ट ही नहीं रहता। यदि उसे सही सात्त्विक लोगों के साथ में रखा जाये तो पलक झपकते ही वह सन्त बन सकता है।
७०
यदि भगवान् न्यायी और दयालु हैं, तब फिर संसार में इतने दुःख और कष्ट क्यों हैं? कई बार हम देखते हैं कि भले लोग कष्ट भोग रहे हैं और धोखेबाज लोग सुख पा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कारण बतायेंगे ?
संसार के कष्ट व्यक्ति की आँखें खोल देते हैं। यदि संसार में दुःख-दर्द न होते तो कोई भी मोक्ष के लिए प्रयत्न न करता। कई बार भगवान् के वरदान ही कष्टों का वेश धारण करके आते हैं।
महात्मा लोग कष्टों को भगवान् के आशीर्वाद के रूप में लेते हैं; क्योंकि यह उनमें सहनशीलता और दया की भावना को विकसित करते हैं और हर समय प्रभु का स्मरण बनाये रखने में सहायता करते हैं। इसीलिए वे कष्टों का स्वागत करते हैं। वे सांसारिक सुख-भोग और समृद्धि को नहीं चाहते। उनका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वे सुख या दुःख-दोनों में ही सदा अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रखते हैं। आप उनकी मनःस्थिति को समझ नहीं सकते। hat a कष्टों में भी प्रसन्न होते हैं। आपका मन अभी सांसारिक है। आप इन बातों को नहीं समझ सकते।
७१
मोक्ष-प्राप्ति के लिए समदृष्टि अनिवार्य बतायी गयी है। इस सम्बन्ध में यदि आप बतायेंगे कि 'अछूतवाद' का क्या महत्त्व है, तो मैं आपका अत्यन्त धन्यवादी होऊँगा। मैं अत्यन्त रूढ़िवादी सिद्धान्तों को मानने वाला हूँ। यदि एक गज दूरी से भी कभी मेहतर या अछूत दिख जाये तो मैं उसी समय स्नान करता और कपड़े धोता हूँ। कृपया बताइए कि क्या इन नियमों का पालन करना चाहिए?
भगवान् से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में वह दिन शीघ्र लायें जब आप किसी झाडू वाले को देखते ही एकता की भावना से भरे हुए उसे हर्षपूर्वक गले लगा लेंगे। वह दिन महान् होगा। आपका हृदय अत्यन्त छोटा, बद्ध और संकुचित है। इसे विशाल बनाने का प्रयत्न करें। धीरे-धीरे 'अछूतवाद' को मन से निकाल दें। नहीं तो यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ी बाधा बन जायेगा। आपको इसमें बहुत अधिक समय लगने की सम्भावना है। 'अछूतवाद' के विचार ने आपके भीतर बहुत गहरी जड़ें जमायी हुई हैं। मानव को मानव से अलग करने वाले इन सब बन्धनों को इसी क्षण कठोरता से तोड़ डालें। आप वर्णनातीत आनन्द एवं परम शान्ति अनुभव करेंगे।
७२
जब कुण्डलिनी जाग्रत हो जाये, तो उसे विभिन्न चक्रों में से होते हुए सहस्रार तक कैसे ले जाया जाता है और फिर योगी जहाँ उसकी इच्छा हो, उस चक्र-विशेष पर उसे कैसे रोक कर रख सकता है? और फिर पुनः विभिन्न चक्रों से होते हुए मूलाधार तक उसे वापस कैसे लाते हैं। कृपया मुझे कुण्डलिनी की गतियों के सम्बन्ध में बताइए।
आपको योनि मुद्रा के अभ्यास के द्वारा कुण्डलिनी को सहस्रार चक्र पर ले जाना पड़ेगा। यदि आप पूरी तरह से इच्छाहीन हो जायें, यदि वासनाओं का पूर्णतया क्षय हो जाये, तो कुण्डलिनी बिना किसी प्रयास के, पवित्रता की शक्ति से अपने-आप ऊर्ध्वगमन कर जायेगी। प्रारब्ध की शक्ति से कुण्डलिनी का स्वयं ही अधोगमन हो जायेगा। यह स्वयं प्रत्येक चक्र पर रुकेगी। आपको इसे कहीं स्थिर करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए अधिक अच्छा होगा कि योग के इन रहस्यों को सीखने के लिए किसी योग्य गुरु के सही निर्देशन में रहें। कुण्डलिनी जाग्रत करने और उसे सहस्रार तक ले जाने का प्रयास करने से पहले पूरी तरह से सदाचारी जीवन जीने का प्रयास करें। फिर जब आप इस पथ पर चल पड़ते हैं और सच्चाई से साधना अथवा योगाभ्यास करने लग जाते हैं, तब आप स्वयं ही जान जायेंगे कि कुण्डलिनी को एक चक्र से दूसरे चक्र पर कैसे ले जाया जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए मेरी पुस्तक 'कुण्डलिनीयोग' को देख सकते हैं।
७३
क्या इस विश्व की संरचना, अणुओं के परस्पर संघात से संयोगवश हुए संगठन से हुई है ? मेरी प्रार्थना है कि मुझे सृष्टि के विकास-क्रम के सम्बन्ध में बताने की कृपा करें।
यह विश्व अणुओं के परस्पर संघात से संयोगवश हुए संगठन का परिणाम नहीं है। विभिन्न दर्शनों के अनुसार सृष्टि के विकास-क्रम के सिद्धान्त अलग-अलग हैं, तथापि इनमें सबसे अधिक मान्यता वेदान्त के सिद्धान्त की है। इसके अनुसार, यह विश्व एक सुव्यवस्थित जैविक इकाई है, जिसको संचालित करने वाली, उसके पीछे निहित एक सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापक सत्ता है। व्यावहारिक दृष्टि से यह दृश्य जगत् सार्वभौम चैतन्य सत्ता के द्वारा प्रेरित की गयी मूल अव्यक्त प्रकृति का क्रमिक विकास है। मूल अव्यक्त प्रकृति के कार्य वस्तुगत दृष्टि से, पंचतन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध), जो कि पंचमहाभूतों (आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी) को जन्म देती हैं, और व्यक्तिपरक दृष्टि से अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार), ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, पंचप्राण और स्थूल शरीर हैं। ये सभी, जो कि अव्यक्त के कार्य हैं, सत्य प्रतीत होते हैं, यद्यपि वास्तव में ऐसा नहीं है; क्योंकि ये सभी कार्य एक ही सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य के ऊपर आधारित हैं। पारमार्थिक दृष्टि से मन की अस्थिर कल्पना के द्वारा बनाये गये एक क्षणिक बाह्य रूप के अतिरिक्त वस्तुतः यह दृश्य जगत् कुछ है ही नहीं।
७४
यदि एक व्यक्ति पूर्ण गुरु है, तो वह एक-साथ ही समय के सभी स्तरों पर कार्य कर सकने में सक्षम होता है। उसमें अतीन्द्रिय-दर्शन एवं अतीन्द्रिय-श्रवण की असाधारण शक्तियाँ होती हैं। अपने विद्यार्थी के बोलने से पहले ही, प्रश्न पूछने के लिए मुख खोलने से पहले ही क्या वह उसके मन की बात नहीं समझ सकता, जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस कर सकते थे? क्या जिसमें ये शक्तियाँ हों, या केवल मन के विचार जान लेने की शक्ति ही हो, उसे गुरु कह सकते हैं?
अतीन्द्रिय-दर्शन और अतीन्द्रिय-श्रवण सदा ही यन्त्रवत् चलती रहने वाली प्रक्रियाएँ नहीं हैं। जब तक गुरु अपना ध्यान किसी की ओर केन्द्रित नहीं करता, तब तक यह आवश्यक नहीं है कि उसे साधक के मानसिक चिन्तन एवं संशयों के सम्बन्ध में जानकारी हो। ऐसे गुरु की दशा की कल्पना करें, जिसे हर समय यह पता चलता रहता हो कि प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है! समाधि की अवस्था में सिद्ध महात्मा सब-कुछ देखता और सुनता है। दूसरे व्यक्ति के विचार जान लेने इत्यादि जैसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेने का अर्थ निश्चित रूप से परिपूर्णता प्राप्त कर लेना नहीं है। साथ ही इन शक्तियों के न होने का अर्थ भी परिपूर्णता प्राप्त न किये होना है। पूर्ण गुरु यदि चाहे, तो ये शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है; किन्तु आप उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
७५
ऐसे व्यक्ति के लिए आपका क्या परामर्श होगा, जिसे परिस्थितिवश दूसरी बार दीक्षा लेनी पड़ गयी हो, किन्तु उसे अभी भी दीक्षा में श्रद्धा न हो ? इसका परिणाम आकर्षण और विकर्षण-दोनों की मिश्रित भावनाओं का उत्पन्न हो जाना है। बचपन से मन में बैठे हुए अच्छे सिद्धान्तों और अब किसी के बताये गये विश्वासों के बीच मन में संघर्ष निरन्तर चलता रहता है और अनिश्चय बना रहता है। ऐसी स्थिति में यदि आत्मा की आवाज कड़ा विरोध प्रकट करे, तो आप क्या परामर्श देंगे ?
अपनी भावनाओं को अथवा मन की स्फुरणाओं को आत्मा की आवाज समझने की गलती न करें। जब पर्याप्त समय तक आप अपने विचारों को शान्त रख सकने की कला में निपुण हो जायें, केवल तभी आत्मा की आवाज सुन सकने की क्षमता प्राप्त हो गयी समझ सकते हैं। और जब यह आपको सुनने लग जाती है, तब आप स्वयमेव ही इसके निर्देशों का अनुसरण करने लग जाते हैं और सभी संशय मिट जाते हैं। दुविधाओं का निवारण करने का एकमात्र उपाय दृढ़निश्चयता है। और जब तक दुविधा रहती है, तब तक दृढ़निश्चय होना कठिन है। आपको अपनी संकल्प-शक्ति का उपयोग करना होगा और परस्पर दुविधा उत्पन्न करने वाले विचारों में से किसी एक-जो आपके विचारानुसार, अथवा जिस पर आपको विश्वास है, के विचारानुसार गलत है-को निकाल फेंकना होगा।
७६
कलिसन्तरणोपनिषद् में यह कहा गया है कि इस कलियुग में पापों के विनाश के लिए एकमात्र उपाय महामन्त्र का जप करना है। किन्तु इस मन्त्र में दो नाम आते हैं, 'हरे राम' और 'हरे कृष्ण' । ये दोनों नाम भिन्न-भिन्न हैं, और यदि भक्त दो अलग-अलग इष्टों का नाम जप करता है, तो क्या यह व्यभिचारिणी भक्ति नहीं हो जायेगी? और फिर, इस मन्त्र का जप करते समय वह भक्त किस के रूप पर मन एकाग्र करेगा, किसका ध्यान करेगा ?
यह व्यभिचारिणी भक्ति के समान नहीं है। व्यभिचारिणी भक्ति तो यह है कि कुछ क्षण भगवान् की पूजा करना और फिर शेष सारा दिन बच्चों, पत्नी, धन-सम्पत्ति इत्यादि को प्रेम करते रहना। राम और कृष्ण के नामों के पीछे आधार स्वरूप परम इष्ट तो एक ही हैं, वह हैं भगवान् विष्णु। ध्यान के लिए आप अपने झुकाव, अभिरुचि अथवा श्रद्धा के अनुसार भगवान् श्री कृष्ण अथवा श्री राम में से जिसको भी चाहें, रख सकते हैं।
७७
शीघ्र आध्यात्मिक सफलता के लिए आप अपने शिष्यों को कैसे प्रशिक्षित करते हैं?
दूषित सांसारिक संस्कारों को पूरी तरह से सुधारने के सशक्त उपाय के तौर पर, मैं अपने विद्यार्थियों को कुछ महीनों या वर्षों के लिए अपने-आपको सक्रिय सेवा में लीन कर देने के लिए कहता हूँ। प्रशिक्षण का समय प्रत्येक विद्यार्थी के विकास के अनुसार अलग-अलग होता है। उन सबको खाना पकाना, बर्तन कपड़े धोना तथा रोगी की देख-रेख करना निश्चित रूप से आना ही चाहिए। उन्हें साधु-संन्यासियों की सेवा हर सम्भव रूप से करनी ही चाहिए। इसके साथ-साथ उनमें सभी योगाभ्यास, एकाग्रता, जप, ध्यान इत्यादि को सीखने की क्षमता आनी चाहिए। उन्हें योग और दर्शन शास्त्र पर लेख लिख सकने की योग्यता निश्चित रूप से विकसित करनी चाहिए। उनको कीर्तन करना तथा प्रवचन देना भी आवश्यक रूप से आ जाना चाहिए। मैं उन्हें इन सबके सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण देता हूँ। उन्हें कुछेक साधारण रोगों के उपचार के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर देता हूँ। और जब यह देखता हूँ कि विद्यार्थी अब अपनी इन्द्रियों पर संयम करने में सक्षम हो गये हैं और धारणा और ध्यान में आगे बढ़ गये हैं, साथ ही अब उनमें समस्त सात्त्विक गुणों का विकास हो चुका है, तब मैं उन्हें गहन ध्यान में उतरने के निर्देशन दे कर किन्हीं शीतल एकान्त स्थलों में भेज देता हूँ।
७८
मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमें क्यों बनाया गया है और फिर बना कर इस दयनीय एवं दुःखद दशा में क्यों डाल दिया गया है? आप तर्क देंगे कि आपका न कभी जन्म हुआ है और न ही कभी मृत्यु होगी। तब फिर हम सब, संस्कारों और माया के पाश से मुक्त अपनी पूर्ण-परिशुद्ध, सर्वशक्तिमान् अवस्था में क्यों नहीं है?
इस प्रकार के प्रश्न, अति-प्रश्न-दुर्बोध प्रश्न हैं-जिनका उत्तर खोजने के लिए, आप भले ही सहस्रों-लाखों वर्ष शिर फोड़ते रहें, किन्तु फिर भी नहीं जान पायेंगे। बुद्धिमान् लोग इस सृष्टि के 'क्यों' और 'कैसे' प्रश्नों के पीछे नहीं जाते हैं। यदि एक छोटा-सा बालक अपने पिता से प्रश्न पूछे, "पापा, आपने मुझे कैसे उत्पन्न किया?" तो पिता जी क्या उत्तर देंगे। वह तो केवल इतना ही कहेंगे, “प्रतीक्षा करो, जब तुम बालक से पुरुष बन जाओगे तब यह अपने-आप समझ जाओगे।" तुम्हारी और तुम्हारे जैसे और बहुत से साधकों, जिनमें प्रकाश प्रवेश करने का अभी प्रयत्न कर रहा है, की यही स्थिति है। गाड़ी को घोड़े के आगे जोतने जैसी उल्टी बात न करें। आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करें। तब आपको ये सब प्रश्न समझ आ जायेंगे। अभी इस समय तो गम्भीरतापूर्वक स्वयं को साधना में लगा दें और मल, विक्षेप एवं आवरण को दूर हटा दें। इन विषयों के सम्बन्ध में व्यर्थ के तर्क-वितकों में न फँसें। आप मुझसे दर्शन शास्त्र के अन्य विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जहाँ-कहीं भी जायेंगे, इस विषय में आपको यही उत्तर मिलेगा। आप मेरी बात समझ गये हैं न?
७९
एक राष्ट्र का चरित्र अपनी भूतपूर्व महिमा में पुनः किस प्रकार उद्भासित हो सकता है?
जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, यह वस्तुतः एक आध्यात्मिक देश है। प्राचीन समय में सर्वत्र आश्रम हुआ करते थे जो दिव्य आदर्शों से स्पन्दित तथा ऐसे श्रद्धास्पद आचार्यों से भरपूर होते थे जो पूर्णतया व्यावहारिक एवं साक्षात्कार प्राप्त किये हुए होते थे। उन आचार्यों के शिष्य तक अत्यन्त उन्नत तथा अपने गुरु के उपदेशों के प्रति अत्यन्त ग्रहणशील थे। इस वर्तमान युग में हास का मुख्य कारण है पश्चिमी सभ्यता की अन्धाधुन्ध नकल। उनके आधुनिक रहन-सहन एवं व्यवहार को बिना यह सोचे-विचारे कि वह हमारी नैतिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में कहाँ तक सहायक हैं और परम परिपूर्णता अथवा मोक्ष, जो कि जीवन का मुख्य एवं एकमात्र उद्देश्य है, को प्राप्त करने में कितने सहायक हैं, उनकी नकल करना है। जो कुछ दूसरों में बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ है, उसका अनुकरण करने की उपेक्षा कर देने में तो आधुनिक व्यक्ति कुशल है; किन्तु जो उसके नैतिक विकास को भ्रष्ट कर देने वाला है, उसे ग्रहण करने को तत्पर रहता है। ऐसी स्थिति में विश्व के हर कोने में, विशेष रूप से भारत में आश्रमों की संख्या में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। आध्यात्मिकता भारत का जन्मसिद्ध अधिकार है, यद्यपि अन्य किसी देश के लिए भी इसमें कोई बाधा नहीं है। अतः भारत को इस दिशा में पहल करनी चाहिए तथा विश्व के उन कोनों, जहाँ भौतिकवाद का अन्धकार व्याप्त है, को प्रकाशित करना चाहिए।
दूसरे, किसी भी धर्म में भेदभाव किये बिना, प्रत्येक के लिए धार्मिक शिक्षा आवश्यक कर दी जानी चाहिए। धार्मिक असहिष्णुता बहुत से युद्धों, शत्रुताओं और मतभेदों इत्यादि का एक कारण रहा है। लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। शास्त्र और धर्म, विज्ञान और धर्म, जुड़वाँ बहनों की भाँति, आधुनिक सांसारिक उन्नति में बिना किसी प्रकार की बाधा पहुँचाये, साथ-साथ चलते रहने चाहिए।
लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कर्म, यदि वह धर्म के विपरीत कर्म नहीं है, तो वह मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में बाधक नहीं है, और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में उन्नति करने की पूरी छूट दी जानी चाहिए। प्राचीन काल की प्रथाएँ, यदि वह विकास-पथ में बाधक नहीं हैं, तो उन्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से जो हमारे भारतवर्ष की प्राचीन महिमा का स्मरण दिलाने वाली हैं। वैज्ञानिक उन्नति के नाम पर उद्योगों के और जीविकोपार्जन के प्राचीन साधनों को पूर्णतया त्याग नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें पहले की तरह चलते रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि केवल उनको बनाये रखने में ही जीवन का नवीनीकरण निहित है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आश्रम जो आदर्श धीर पुरुषों का निर्माण करें, उन्हें चाहिए कि वे समय-समय पर अपने आश्रमवासियों को यात्राओं पर भेज कर आत्मज्ञान का प्रचार-प्रसार करें।
समय-समय पर आध्यात्मिक सम्मेलन किये जाने चाहिए तथा साधना की विधियों अथवा अनुष्ठानों के विषय में बताया जाना और करवाया जाना चाहिए। ऐसी सुधारवादी प्रक्रियाएँ चलती रहनी चाहिए, केवल भारत में ही नहीं प्रत्युत् समस्त संसार में हर स्थान पर चलती रहनी चाहिए। और भगवान् की इच्छा है कि इसमें भारतवर्ष अग्रणी बने। अब यह भारतवासियों का पावन कर्तव्य बन जाता है कि इसे तत्काल प्रारम्भ कर दें।
८०
धूम्रपान कैसे बन्द किया जाये ?
आदत का परित्याग कर दें। स्नायविक उत्तेजना को प्रभावहीन करने के लिए कोई शामक औषधि ले लें। धूम्रपान करने वाले साथियों से दूर रहें। अपने मन को किसी-न-किसी काम में व्यस्त रखें। मन को खाली एवं निष्क्रिय न छोड़ें। स्वच्छता के नियमों, अच्छे स्वास्थ्य के सिद्धान्तों तथा आदर्श-जीवन के नियमों के विषय में पढ़ें। मानव-प्रणाली पर तम्बाकू के विनाशकारी प्रभाव के सम्बन्ध में अपने मन को भली-भाँति समझाते रहें। सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें तथा उनके ऊपर मनन करें। योगासन-प्राणायाम का अभ्यास करें। भगवान् का स्मरण हर समय करते रहें। सभी दुर्गुण अपने-आप नष्ट हो जायेंगे।
८१
भगवद्गीता में बहुत से उन विषयों के सम्बन्ध में बताया गया है, जो ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त लाभदायक हैं; किन्तु आश्चर्य की बात है कि सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य के सम्बन्ध में कुछ भी चर्चा नहीं की गयी है। भगवान् ने सृष्टि की रचना आरम्भ ही क्यों की?'
सृष्टि की रचना के उद्देश्य सम्बन्धी गीता में भगवान् का मौन यथार्थ में उनके दिव्य विवेक का प्रकटीकरण है। यही प्रश्न विभिन्न मस्तिष्कों में विभिन्न रूपों में उठा करता है। ब्रह्म में अविद्या का उदय कैसे हुआ? कर्म कब आरम्भ हुए? निराकार ब्रह्म ने आकार क्यों धारण किये ? परम प्रकाश में अज्ञान का अन्धकार अथवा माया का अस्तित्व कैसे हो सकता है? ये सब, तथा ऐसे ही अन्य अनेकों प्रश्न उठते हैं। इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं हो सकता। इसमें उस 'परम तत्त्व' की पूर्ण जानकारी निहित है, जो इन सब प्रश्नों के पीछे तथा परे है, जो समस्त कारणों का मूल कारण, समस्त विषयों का मूल विषय है। यह किसी विषय-वस्तु की भाँति नहीं जाना जा सकता। और जब सबका 'मूल विषय' (निज आत्म-तत्त्व) स्वयं को जान लेता है, तब वाणी और विचार समाप्त हो जाते हैं। संशय संशयकर्ता में लीन हो जाता है। उस परम मौन में प्रश्नों का समाधान अनिर्वचनीय रूप से हो जाता है। समस्या सुलझ जाती है; किन्तु वाणी विस्मित हो कर मूक रह जाती है-और प्रश्न अनुत्तरित ही रहता है।
अतः भगवान् गीता में इस लोकोत्तर प्रश्न के सम्बन्ध में मौन हैं; किन्तु वह सर्वशक्तिमान् परमात्मा इस प्रश्न का उत्तर जानने के मार्ग एवं साधन बता देते हैं। सृष्टि की संरचना क्यों की गयी, इसकी चिन्ता न करें; अपितु सृष्टिकर्ता को जानने का प्रयास करें। संसार जैसा है, उसमें रहते हुए उससे अतीत जाने का प्रयत्न करें। इसी में बुद्धिमत्ता है। बौद्धिक स्तर से इस रहस्य को जानने का प्रयत्न करना केवल मानसिक निराशा प्राप्त करना मात्र ही है।
लोकातीत विषयों में कोई 'क्यों' नहीं है। 'क्यों' तो केवल लौकिक वस्तुओं का होता है। तर्क सीमित एवं नश्वर है। 'क्यों' तो केवल भगवान् ही जानते हैं। आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करें, तब आपको उत्तर मिल जायेगा, तब आप माया का तथा अन्य सबका मूल उद्गम एवं प्रकृति जान जायेंगे।
८२
गाँधी जी की हत्या के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं?
दैवी इच्छा ही सब ओर कार्यान्वित है। देह छूट जाने का अर्थ व्यक्ति की मृत्यु नहीं है। यदि व्यक्ति चाहे तो वह शरीर छूट जाने के बाद भी अपना कार्य पूर्ण कर लेगा। किसी भी कार्य को करने वाला केवल यह शरीर नहीं होता। वास्तव में जो कर्ता है, उसका किया गया कार्य कभी नष्ट नहीं होता। केवल शरीर की हत्या कर देने से उसे किसी भी कार्य को करने से रोकना सम्भव नहीं है। गाँधी जी गीता के द्वितीय अध्याय के उपासक थे और उनका दृढ़ विश्वास था कि उनमें संस्थित निज स्वरूप आत्मा अनश्वर है।
८३
आप कहते हैं, "आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है और हम वास्तव में सर्वव्यापक एवं परिपूर्ण हैं।" आप यह भी कहते हैं, "जीव आत्मा में वैयक्तिकता (अलगाव) का भाव है; किन्तु परम आत्मा में नहीं....." प्रश्न
उठता है-क्या आत्म-तत्त्व दो हैं? एक वैयक्तिक भाव में फँसा हुआ और दूसरा व्यक्तिपरक न हो कर समष्टिपरक ?
वास्तव में आत्मा एक ही है जो निरपेक्ष अथवा असीम है। सापेक्ष आत्मा परिपूर्ण आत्मा से अलग नहीं है; किन्तु यह केवल निरपेक्ष आत्म-तत्त्व को, उपाधियों के अथवा मन के माध्यम से देखना है। किसी भी वस्तु का अपना एक स्वतन्त्र निज स्वभाव होता है; किन्तु जब उसे विकृत रंगीन शीशे में से देखा जाये तो वह वस्तु भी विकृत और रंगीन दिखायी देती है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वस्तु एक ही समय में सही और विकृत-दोनों है; अन्तर केवल यह है कि हम इसे किस माध्यम से देखते और ज्ञान प्राप्त करते हैं। निरपेक्ष आत्मा को सीमित मन के माध्यम से अनुभव करने तथा मन को ज्ञान का उपकरण बनाने में भी यही बात है। सार्वभौम निरपेक्ष सत्ता एक ही है, भेद हमारे बोध (ज्ञान) के माध्यम का है।
८४
मैं अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि लोगों के प्रति अपने व्यवहार में भलाई करने से सदा लाभ नहीं होता। फिर भले होने और भला करने का क्या लाभ है जब भलाई को न तो कोई कुछ समझता है न ही उसका कुछ सही लाभ होता है? कृपया आप इस पर प्रकाश डालें।
लौकिक दृष्टि से भले ही भलाई आपको कुछ लाभ पहुँचाये या नहीं, फिर भी आप सदा भलाई करें और भले ही रहें। इसमें सन्देह नहीं कि सांसारिक लोग सामान्यतया ऐसे भोलेभाले लोगों को अपनी इच्छापूर्ति करने और कई बार ठग लेने के लिए भी, आदर्श व्यक्ति समझते हैं। किन्तु इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान् तो हमेशा भलाई के साथ हैं, और जो धर्म पर दृढ़ रहता है तथा भगवान् पर भरोसा रखता है, उसी के साथ भगवान् रहते हैं। दया के सद्गुण के बिना तथा गलत कार्य करने से भगवान् का भय होने के स्वभाव के बिना किसी को भला आदमी नहीं कहा जा सकता। भलाई एवं दया साथ-साथ चलते हैं।
भला व्यक्ति संसार में रहता है; किन्तु हमेशा उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर ही होता है। वह व्यावहारिक पुरुष जैसा नहीं होता। भले होने का अर्थ है पवित्रता तथा परमात्मा के प्रति भक्ति-भावना को प्रचुर मात्रा में विकसित करना। भला करने से आप अपने लिए भलाई का बीज बो देते हैं। यदि एक भला कार्य किया जाता है तो आपके लिए उसका मधुर फल उत्पन्न हो जाता है और आपने चाहा हो अथवा न चाहा हो, उसका सुखद भोग आपको प्राप्त होता ही है। यदि कोई बुरा कर्म किया जाता है तो उसके फलस्वरूप आप चाहें या न चाहें, कड़वा एवं विपरीत फल आपको भोगना ही पड़ेगा। आपकी भलाई को भले ही कोई मान्यता दे या न दे, आप आजीवन भला करते जायें और भले ही बनें। केवल इसी के द्वारा आपको चित्तशुद्धि तथा उसके उपरान्त आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। सांसारिक रुचियों वाले लोग, जिन्हें आत्मा सम्बन्धी कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल वही हैं जो यह नहीं समझते कि भलाई करने से ही धीरे-धीरे विकसित होता हुआ मानव परिपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक अभिरुचि के लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वह भली-भाँति इस बात को समझते हैं कि भला करने और भले होने से उन्हें जीवन का लक्ष्य अर्थात् परमात्म-साक्षात्कार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
इसे स्मरण रखें कि भगवान् भला करने और भला व्यक्ति बनने को ही महत्त्व देते हैं। और सदैव उसका फल प्रदान करते हैं। वास्तव में तो वह उन्हीं लोगों में निवास करते और उन्हीं के साथ रहते हैं। भला व्यक्ति सचमुच स्वयं में उनकी विद्यमानता को, तथा सर्वत्र उनकी उपस्थिति को बिना किसी संशय के अनुभव करता है। अपने में, अपने साथ और अपने चारों ओर भगवान् की उपस्थिति के प्रति जाग्रत रहे बिना स्वयं को भला व्यक्ति समझ लेना तो उपहास मात्र ही है। यदि भला होने पर और भले कार्य करने पर लोग महत्त्व नहीं देते तो भला बनने एवं भला करने के लाभ पर प्रश्न न करें, क्योंकि कार्य करना मनुष्य के हाथ में है, उसके भले या बुरे फल पर उसका अधिकार नहीं है।
८५
यदि राजनीतिज्ञ न हों, तो क्या विश्व में शान्ति हो जायेगी ?
राजनीतिज्ञों के होने अथवा न होने पर विश्व की शान्ति निर्भर नहीं करती। यदि लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से परिपूर्ण रूप से धर्म, विवेक, सत्य और न्याय के सिद्धान्तों को समझ कर जीवन जीते हैं, तो उस पर यह निर्भर करती है। जब तक लोग इस स्तर तक ऊपर नहीं उठते, तब तक जो शासन को चलाने वाले हैं, वे अपने स्वार्थ एवं लोभ से प्रेरित होते हुए उसी के अनुसार कार्य करते रहेंगे तथा करोड़ों लोगों की भावनाओं एवं कष्टों की ओर ध्यान न देते हुए उन्हें कुचलते रहेंगे तथा युद्धों को आमन्त्रित करते रहेंगे, भले ही यह युद्ध कितने भी विनाशकारी क्यों न हों।
८६
मैं पिछले पाँच वर्षों से कठोर तप और ध्यान कर रहा हूँ। किन्तु यह सब करने पर मैंने पाया है कि मेरे संकट और समस्याएँ बढ़ती ही जा रही हैं। मेरी नौकरी चली गयी है, मैं भुखमरी झेल रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ ? क्या यही भगवान् की कृपा है? अपनी साधना मैं कैसे चलती रख सकता हूँ, जब मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं है?
कहते हैं कि भगवान् तो चट्टानों की परतों में रहने वाले मेंढक तक को भी भोजन देते हैं। केवल आपके सम्बन्ध में ही वह कैसे असफल हो गये? यह सचमुच आश्चर्य की बात है! क्या वे अपने कर्तव्य को पूरा करने से चूक गये हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। वह तो पूर्ण रूप से दयामय हैं, सबके हितैषी हैं! वास्तव में वह आपमें साहस, प्रत्युत्पन्नमति, सहनशीलता, सुदृढ़ आत्म-बल, धैर्य, दया और प्रेम जैसे उन सद्गुणों को विकसित करना चाहते हैं जिनके द्वारा उनका यह उपकरण (आप) उनकी दिव्य लीला के लिए पूर्णतया उपयुक्त बन जाये। हाँ, निश्चित रूप से यही बात होगी।
संघर्षरत एवं सच्चे साधक को इसलिए भी अधिक मुसीबतों और कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें परम शान्ति और परिशुद्ध आनन्द के साम्राज्य को प्राप्त करने के पथ पर शीघ्रता से अग्रसर होना होता है।
राजपरिवार की राजकुमारी मीरा ने वैभवपूर्ण महलों के सुख-ऐश्वर्य से पूर्ण जीवन को त्याग दिया और राजपूताना की जलती रेतीली धरती पर निकल पड़ी। वृन्दावन के मार्ग में चलते समय उसने भूख-प्यास को सहन किया। वह धरती पर सोयी, भिक्षावृत्ति पर जीवन-निर्वाह किया। पाण्डवों के सहायक भगवान् श्री कृष्ण थे, तो भी उन्हें असंख्य कष्टों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी की रक्षा करने वाले भीम, अर्जुन और स्वयं धर्मपुत्र युधिष्ठिर के होते हुए भी उसे अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में से गुजरना पड़ा था। जिन कष्टों में से पाण्डवों को, श्री राम को और मीरा को निकलना पड़ा था उन सब कष्टों के सामने हमारे कष्ट तो कुछ भी नहीं हैं। राजा हरिश्चन्द्र और उनकी धर्मपत्नी की मुसीबतों की ओर देखें! उन्हें सत्य का पालन करने के लिए श्मशानभूमि में दास बन कर चाण्डाल का काम करना पड़ा। ये कष्ट ही मनुष्य के आत्म-बल को सुदृढ़ एवं विकसित करते हैं। केवल कष्ट सहन करने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलने में सक्षम होता है। चिन्तित न हों! प्रत्येक पग पर भगवान् शिव की कृपा एवं दया को अनुभव करें। सभी कठिनाइयाँ इस प्रकार समाप्त हो जायेंगी जैसे सूर्य की गरमी के सामने कोहरा समाप्त हो जाता है। परमात्मा की कृपा में पूर्णतया अडिग विश्वास रखें।
८७
वास्तविक एवं सच्चे गुरु के क्या चिह्न हैं? क्या साधारण मनुष्य के लिए यह सम्भव है कि वह वास्तविक गुरु का चयन कर सके ? यदि ऐसा सम्भव है, तो वह कैसे यह करे ?
जो सद्ग्रन्थों का ज्ञाता अर्थात् श्रोत्रीय हो एवं जो ब्रह्म में पूर्णतया प्रतिष्ठित अर्थात् ब्रह्मनिष्ठ हो, वही वास्तविक गुरु होता है। जो व्यक्ति विवेकशील, कामनाओं से रहित तथा निष्पाप हो, वह सच्चा गुरु हो सकता है। ऐसा गुरु अपने ज्ञान एवं सक्षमता के द्वारा उन प्राणियों को अपनी ओर स्वयं ही खींच लेता है, जिन्हें निर्देशित करने के लिए वह उपयुक्त समझता है। जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि वह किसी ऐसे महापुरुष की ओर स्वतः ही खिंचा चला जा रहा है जिसे प्रेम किये बिना, जिसकी प्रशंसा और सेवा किये बिना वह रह नहीं सक रहा, जो अविक्षुब्ध प्रशान्तावस्था, करुणा एवं आध्यात्मिक अनुभूति की साकार प्रतिमा है, तो ऐसे महान् व्यक्ति को गुरु बनाया जा सकता है। गुरु वह है जिसमें शिष्य कोई भी कमी न ढूँढ़ सके और जो शिष्य के लिए उस आदर्श पर प्रतिष्ठित हो, जहाँ शिष्य को पहुँचना है। संक्षेप में, वास्तविक गुरु भगवान् का प्रकटित स्वरूप होता है और जिस मनुष्य में परिपूर्ण दिव्यता अभिव्यक्त होती हो, उसे गुरु के रूप में चयन किया जा सकता है। गुरु और शिष्य का परस्पर सच्चा और अटूट सम्बन्ध है, बिलकुल उसी प्रकार से जैसे मनुष्य और भगवान् के मध्य होता है। यह प्राकृतिक नियम है कि विश्व में जब भी कोई घटना होनी होती है, तो बिलकुल उस निश्चित समय पर उसके अनुसार वैसी ही परिस्थितियाँ बन जाती हैं। जब शिष्य उच्चतर प्रकाश ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तब उस समय परमात्मा के विधानानुसार उसका सम्पर्क उसके अनुकूल गुरु से हो जाता है।
८८
मन का आत्मा से क्या अन्तर है?
आत्मा, जो कि असीम और सर्वदा एवं सदा सर्वव्यापक है, का मन एक विशेष सीमित व्यक्तित्व रूप अथवा परिच्छिन्न इकाई है। मन असंख्य इच्छाओं का समूह है, इसलिए यह जड़ और शक्तिहीन है। किन्तु यह चेतन और शक्तिशाली इसलिए प्रतीत होता है, क्योंकि चेतन आत्मा का प्रकटीकरण इसके माध्यम से होता है, वास्तव में केवल मन ही मनुष्य का असली व्यक्तित्व है और यह समस्त कार्यों का वास्तविक कर्ता है। संसार की सभी घटना-परिस्थितियों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कर्ता-भोक्ता यह मन ही है। आत्मा अपने-आपमें परिपूर्ण है और मन के किसी भी अनुभव से अप्रभावित रहती है। मन नश्वर है, जब कि आत्मा अमर है।
८९
हमारे सन्त एवं तपस्वी महात्मा व्याघ्र अथवा मृग-चर्म को उपयोग में लाते हैं। क्या पशु की हत्या करना अथवा करवाना और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो आध्यात्मिक पथ पर इतना उन्नत हो चुके हों, पाप नहीं है? मृत पशु के चर्म पर बैठ कर अपनी मुक्ति की आकांक्षा रखना क्या एक साधु के लिए उचित है ?
इसमें सबसे आवश्यक इस बात को समझना और याद रखना चाहिए कि आसन के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले मृग अथवा व्याघ्र-चर्म को प्राप्त करने के लिए कभी भी उस पशु की हत्या नहीं की जाती। मृग सदा ही संन्यासियों और महर्षियों के आश्रमों का एक अंग हुआ करते थे और जब यह मृग अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होते होंगे तभी यह चर्म, जो कि वनों में प्राप्त करने में सुविधाजनक भी रहता होगा, ले लिया जाता होगा। उस समय वनवासी साधु-तपस्वियों के लिए वस्त्र की अपेक्षा मृग-चर्म अथवा वृक्षों की छाल अधिक सरलता से उपलब्ध हो जाती थी।
व्याघ्र-चर्म को भी इसी ढंग से प्राप्त किया जाता था, किन्तु अधिकांश रूप में तो मृग-चर्म ही प्रयोग में लाया जाता था। वैसे भी मृग-चर्म को आसन के रूप में उपयोग में लाना बताया गया है।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तपस्वी सन्तों ने अनुभव किया है कि मृग-चर्म आसन-रूप में प्रयोग करना समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अत्यन्त अनुकूल है। साधना से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ मृगचर्म के आसन द्वारा अधिक सुरक्षित रहती हैं।
९०
क्या मैं पुस्तकों की सहायता से प्राणायाम कर सकता हूँ?
हाँ! किन्तु उनमें दिये गये निर्देशनों को पूरी तरह से और कई बार पढ़ना एवं समझना अत्यन्त आवश्यक है। यदि कहीं पर कोई संशय अथवा अस्पष्टता आपको लगती हो तो किसी अच्छे जानकार एवं अनुभवी व्यक्ति से पूछ कर फिर अभ्यास आरम्भ करें। नियमित रूप से विधिवत् अभ्यास करें। यदि आप शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं तो आपको मेरी पुस्तक 'साइंस ऑफ प्राणायाम' (प्राणायाम-साधना) के प्रथम दो अध्यायों में दिये गये निर्देशनों का भलीभाँति अनुसरण करना चाहिए। आप कुम्भक का समय धीरे-धीरे बढ़ा कर दो मिनट तक ले जा सकते हैं। अधिक आगे के स्तरों में पहुँचने के लिए गुरु की सहायता लेना अधिक अच्छा रहेगा।
९१
क्या विवाहित महिला बिना किसी हानि के प्राणायाम का अभ्यास कर सकती है?
योगाभ्यास, किसी भी प्रकार का हो, स्त्री-पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। जो अभ्यास शरीर से सम्बन्धित हैं जैसे हठयोग अथवा कुण्डलिनीयोग, इनमें महिलाओं को शारीरिक भिन्नता एवं सीमितताओं के कारण कुछेक सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्राणायाम-साधना के लिए महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है।
९२
भगवद्गीता की शिक्षा युद्ध के मैदान में क्यों दी गयी थी ?
गीता उपदेश के लिए युद्धभूमि का चुनाव करने में निश्चित रूप से भगवान् का कुछ विशेष कारण था। वे हमें समझाना चाहते थे कि विवेकशीलता अथवा ज्ञान आरामकुर्सी पर बैठ कर या लेटते समय के लिए नहीं होना चाहिए। यदि संघर्ष-काल में ज्ञान व्यक्ति का साथ नहीं देता तो वह ज्ञान है ही नहीं! भरे पेट से, आराम से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति दर्शनशास्त्र की चर्चा कर सकता है। आराम से आग तापते हुए तो कोई भी व्यक्ति योगशास्त्र सम्बन्धी कठिन से कठिन विषय पर प्रवचन कर देगा। किन्तु यह तो विवेक नहीं है, यह तो परम ज्ञान के सम्बन्ध में दिखावटी अथवा मौखिक ज्ञान मात्र ही है। यह पाखण्ड है। ऐसे लोग जब परीक्षा का समय होता है, जब उनके ज्ञान को व्यवहार क्षेत्र में उतर कर कष्टों का सामना करना पड़ता है, तब वह बुरी तरह से असफल हो जाते हैं।
भगवान् श्री कृष्ण का पांचजन्य जोर से गर्जन करते हुए कहता है, नहीं! नहीं, नहीं, यह ज्ञान नहीं है; वास्तविक ज्ञान, सच्चा विवेक आपकी युद्धभूमि में भी भलीभाँति सहायता करेगा, पूर्ण संकटकालीन परिस्थितियों में आपके साथ रहते हुए आपको समस्याओं से उबरने में सक्षम बनायेगा, आपकी मुसीबतों में, उनको सुलझाने की शक्ति देगा, प्रलोभनों में न फँसने की क्षमता देगा और परीक्षा की घड़ियों में विजयी बनायेगा। कठिनाइयों को परिवर्तित करते हुए आप उन्हें अपनी विलक्षणता सिद्ध करने का सुअवसर बना लेंगे; क्योंकि प्रायः कठिन परिस्थितियाँ ही व्यक्ति को महान् बनाने का कारण बन जाती हैं।
प्रलोभन और परीक्षाएँ भले ही कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हों, सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति उनसे पराजित नहीं होते, प्रत्युत् इसके विपरीत केवल ऐसे अवसरों पर ही उनकी शक्ति प्रकट होती है। दुर्बल मानसिकता वाला व्यक्ति उस समय तो दर्शन-शास्र की बात करता है, जब सब-कुछ उसकी इच्छाओं के अनुकूल चल रहा हो, किन्तु परीक्षा की घड़ी आते ही सारी की सारी दार्शनिकता पंख लगा कर उड़ जाती है। जब कि सुदृढ़ मानसिकता सम्पन्न व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में अपनी योग्यता का भले ही प्रदर्शन न करता हो, किन्तु जब संकट उपस्थित हो जाता है, तब वह अपनी सामर्थ्य अभिव्यक्त करके आश्चर्यचकित कर देता है।
भगवान् श्री कृष्ण को अपने प्रवचन के लिए युद्ध के मैदान का चयन करने के पीछे निहित इस आशय को साधकों को समझना चाहिए। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने समस्त मानव-जाति को जो महान् समत्वयोग के विषय में ज्ञानोपदेश देना था मानो यह स्थान ही उसके लिए अत्यन्त उपयुक्त प्रस्तावना थी।
९३
मैं पूरा आधे घण्टे का शीर्षासन का अभ्यास कर रहा हूँ; किन्तु मैं स्वप्न-दोष से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। मेरी साधना में क्या कमी है? कामवासना को कैसे नष्ट करूँ?
शीर्षासन का दीर्घ काल तक का अभ्यास निःसन्देह आपकी कामवासनाओं को नष्ट करने में बहुत सहायता करेगा; किन्तु इसके साथ ही आपका चिन्तन भी शुद्ध होना चाहिए। किसी भी कामुक विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। सत्संग करें। सात्त्विक आहार लें। स्त्रियों की ओर न देखें। अपने में वैराग्य विकसित करें। इन्द्रियों को संयमित करें। यदि आप निश्चित सफलता पाना चाहते हैं, तो इन सब निर्देशों का पालन करना होगा। यदि आप कामुक विचारों को पोषित करते रहते हैं, यदि कामी पुरुषों का साथ करते हैं, यदि आप शुद्ध सात्त्विक भोजन नहीं लेते, फिर अपनी कामवासना को कैसे नष्ट कर सकते हैं, भले ही क्यों न तीन घण्टे तक शीर्षासन करते रहें?
९४
मैंने अभी ही संन्यास लिया है। क्या मैं परिव्राजक जीवन जी सकता हूँ अथवा मुझे एकान्तवास करना चाहिए?
नये संन्यासी के लिए कठोर साधनापूर्वक छह वर्ष तक पूर्णतया एकान्तवास करना आवश्यक है। यह आपकी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। परिव्राजक जीवन में विधिवत् साधना नहीं का जा सकती। सब जगह विक्षेप अथवा विकर्षण रहते हैं। कुछ वर्षों तक आपको विषय-पदार्थों से दूर रहना चाहिए। कठोर एकान्तवास से बहुत लाभ होगा। वर्ष में एक बार, कुछ दिन के लिए ऋतु-परिवर्तन के लिए किसी दूसरे स्थान पर आप जा सकते हैं। यदि लगे कि आप तमस् में प्रवेश करने लगे हैं, तो तुरन्त सक्रिय सेवा में लग जाना चाहिए। आरम्भ में दो या तीन वर्ष के लिए निष्काम सेवा कार्य अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद पूर्ण एकान्त। बीच-बीच में कभी कुछ दिन के लिए, अपने मन की सुदृढ़ता की परीक्षा के उद्देश्य से परिव्राजक जीवन अपना सकते हैं।
९५
मैं विवाहित पुरुष हूँ। संन्यासी बनने की मेरी अति तीव्र चाह है। पारिवारिक जीवन से मुझे विरक्ति हो गयी है। अभी हाल ही में मेरे बच्चे की मृत्यु हो गयी है। मेरी धर्मपत्नी भी एक धर्मपरायण महिला है। यदि मैं संन्यास ले लूँ, तो क्या मैं अपनी पत्नी के साथ रहते हुए आध्यात्मिक साधना कर सकता हूँ?
अभी आपके लिए संन्यास लेना उचित नहीं है, भले ही पुत्र की मृत्यु के कारण आपके मन में किंचित् वैराग्य उत्पन्न हुआ हो। संन्यास लेने के बाद आपको अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहिए। आपको तो वस्तुतः अपने घर में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके मन के एक कोने में मोह अभी भी छिपा बैठा है। पुराने सांसारिक संस्कार आपको छलने के लिए घात लगाये बैठे होंगे। माया अत्यन्त शक्तिशाली है। आपको अपनी सारी शक्ति पुराने संस्कारों एवं लालसाओं के साथ गुप्त-संघर्ष करने में खर्च करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक साधनाएँ करने के लिए शक्ति ही शेष नहीं बचेगी। भले ही आप यह सोचते हैं कि आपमें उच्चकोटि का वैराग्य आ गया है और आपकी धर्मपत्नी भी धर्मपरायण नारी है, तो भी आपको उससे बहुत दूर रहना होगा। उसके सम्बन्ध में सोचना तक भी नहीं होगा। यह सच्चा संन्यास है। संन्यास लेना और पत्नी के साथ रहना, यह कैसा संन्यास है! इस तरह आप मोह और सांसारिक संस्कारों एवं वासनाओं को कैसे नष्ट करेंगे ?
९६
कई बार जुकाम अथवा ऐसे ही किसी-न-किसी कारण से, मेरी कोई एक नासिका बन्द हो जाती है और श्वास अच्छी तरह से नहीं आता, जिसके कारण प्राणायाम करने में कठिनाई लगती है। श्वास-प्रश्वास की गति अबाध करने के लिए मैं क्या करूँ?
अपनी बन्द नासिका में धागे का एक सिरा (किनारा) डालें। आपको छींकें आने लगेंगी। इससे आपकी बन्द नासिका खुल जायेगी। या फिर जो नासिका बन्द हो, उसके विपरीत करवट ले कर पाँच मिनट के लिए लेट जायें। इससे भी श्वास ठीक आने लगेगा। भस्त्रिका प्राणायाम को चार बार करें, आप ठीक हो जायेंगे।
९७
जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद (अन्तर) है?
अविद्या अथवा मन में प्रतिबिम्बित आत्मा-जीवात्मा है। परमात्मा परम-आत्मा, ब्रह्म अथवा शुद्ध आत्मा है। आनुभाविक दृष्टिकोण से, जीवात्मा सीमित और सोपाधिक है, जब कि परमात्मा असीम, शाश्वत, सत्-चित्-आनन्द ब्रह्म है। तत्त्वतः जीवात्मा- अविद्या के नष्ट हो जाने पर-परमात्मा से अभिन्न है।
९८
भगवान् ने सुन्दर युवतियों की सृष्टि क्यों की है? उनकी इस सृष्टि-रचना के पीछे निश्चित रूप से कोई कारण होगा ही। हमें उनका सुख-भोग करना चाहिए और जितनी भी हो सके, सन्तानोत्पत्ति करनी चाहिए। हमें वंश-परम्परा को चलते रखना चाहिए। यदि सभी लोग संन्यासी हो कर वनों में चले जायेंगे तो संसार का क्या होगा ?
ये सुन्दर युवतियाँ और धन-दौलत आपको अपने जाल में फँसाने के लिए माया के उपकरण हैं। यदि आप सदा निम्न विचारों, दूषित इच्छाओं वाले सांसारिक मनुष्य ही रहना चाहते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता से रहें, आपको पूर्ण स्वतन्त्रता है। आप तीन सौ पचास स्त्रियों से विवाह करें और जितनी इच्छा हो, उतनी सन्तानोत्पत्ति करें। कोई आपको नहीं रोकता। किन्तु शीघ्र ही आपको ज्ञात हो जायेगा कि जो सन्तुष्टि आप पाना चाहते हैं, वह संसार आपको नहीं दे सकता; क्योंकि सभी वस्तु-पदार्थ देश, काल और समय की सीमा में आबद्ध हैं। यहाँ पर मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, चिन्ताएँ, तनाव, भय, हानि, निराशा, असफलता, अप्रिय कटु भाषण, गरमी, सर्दी, सर्प-दंश, वृश्चिक-दंश, भूकम्प, दुर्घटनाएँ इत्यादि सब-कुछ है। एक क्षण के लिए भी आपको मानसिक शान्ति नहीं मिल सकती। अभी आपका मन वासनाओं और अपवित्रता से भरा हुआ है, इसलिए आपकी विचार एवं विवेक-बुद्धि मलिनता से आच्छादित एवं विपरीत हो गयी है। आप जगत् की भ्रामक प्रवृत्ति को तथा आत्मा के शाश्वत आनन्द को समझने की क्षमताओं को खोये हुए हैं।
वासना को अत्यन्त शक्तिशाली ढंग से नियन्त्रित किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सशक्त उपाय हैं। वासना को नियन्त्रित कर लेने पर, आप अपने भीतर से, आत्मा से वास्तविक आनन्द को प्राप्त करेंगे।
सब लोग संन्यासी नहीं बन सकते। उनके अनेकों बन्धन और आसक्तियाँ हैं। वे वासनाओं से भरे हुए हैं; अतः संसार का त्याग नहीं कर सकते। वे अपनी पत्नियों, बच्चों और धन-सम्पत्ति से जकड़े हुए हैं। आपका तर्क पूर्णतया गलत है। यह असम्भव है। क्या आपने अतीत से अब तक के किसी इतिहास में ऐसा सुना है कि सभी मनुष्य संन्यासी हो गये हैं और संसार निर्जन हो गया ? फिर आप ऐसा बेतुका तर्क क्यों कर रहे हैं? आपके मूर्खतापूर्ण विचार और शैतानी दर्शन, जो अपने में वासना और कामुक वृत्तियों को लिये हुए हैं, को सही सिद्ध करने की, यह आपके मन की चालाकी है। भविष्य में कभी इस प्रकार की बात न करें, क्योंकि इससे आपकी मूर्खता और कामुक वृत्ति प्रकट हो जायेगी। इस संसार के लिए चिन्ता न करें। अपने सम्बन्ध में सोचें। भगवान् सर्वशक्तिमान् हैं, यदि सभी लोग संन्यासी हो कर वन-गमन कर भी जाते हैं, और यह जगत् पूर्णतया निर्जन हो जाता है, तो भी भगवान् केवल अपनी इच्छा मात्र से ही पल भर में करोड़ों लोगों की सृष्टि कर देंगे, पलक झपकते ही कर देंगे। यह आपकी चिन्ता का विषय नहीं है। आप तो अपनी काम-वासना को दूर करने के उपाय खोजिए।
९९
आत्मा किस मार्ग से शरीर छोड़ कर जाती है?
जब तक प्राण ऊर्ध्वगमन करते हैं और अपान निम्नगमन करते रहते हैं, तब तक जीवन चलता रहता है। किन्तु, जैसे ही दोनों में से एक निर्बल हो जाता है, तब जीवन-शक्ति देह छोड़ जाती है। यदि उस समय अपान दुर्बल है, तो जीव या तो शिर या नासिकाओं, या कान और मुख से निकलता है। यदि प्राण दुर्बल हो तो यह मलद्वार से बाहर निकलता है।
१००
सूक्ष्म शरीर क्या है ?
इस स्थूल भौतिक शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, जो इस प्रकार है जैसे फुटबाल के भीतर 'ब्लैडर' अर्थात् वायु भरने वाली रबड़ की थैली रहती है। यह भौतिक शरीर की पूर्णतया प्रतिमूर्ति अथवा पूरक है। यह पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से निर्मित है। कुछ इसे 'दी डबल' (द्विक) कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर ही मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर उसके स्थूल शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक को गमन करता है। उस 'परम सत्य' की ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर का अन्त हो जाने से ही व्यक्ति जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है।
१०१
भारत में ७० लाख साधु हैं और करोड़ों रुपये इन साधुओं को खिलाने-पिलाने में नष्ट हो रहे हैं। प्रत्येक साधु या संन्यासी समाज के ऊपर परजीवी के रूप में भार बना हुआ है। संन्यासी होने पर भी उसे राजनैतिक क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। एकान्त जीवन जीने की अथवा संन्यास परम्परा अपनाने की अथवा निवृत्ति मार्ग अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल कार्यकर्ताओं की ही आवश्यकता है।
यह एक शोकपूर्ण गलती है। यह जनगणना झूठी है। संन्यासियों और साधुओं की सूची में भिखारियों को सम्मिलित कर लिया गया है। वास्तविक संन्यासी गिने-चुने और दुर्लभ हैं। उनकी संख्या तो उँगलियों पर गिनी जा सकती है। केवल एक वास्तविक संन्यासी ही इस पृथ्वी का सम्राट् है। वह कभी कुछ लेता नहीं। वह तो सदैव देता ही है। वह संन्यासी ही थे, जिन्होंने अतीत काल में महिमामयी उदात्त कार्य किये। केवल संन्यासी ही हैं जो वर्तमान में और भविष्य में भी महान् एवं विलक्षण कार्य कर सकते हैं। जब तक यह संसार है, तब तक श्री शंकराचार्य का नाम कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। यह स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ही थे, जिन्होंने सद्ग्रन्थों की उदात्त शिक्षाओं का प्रचार किया और हमारे धर्मग्रन्थों को सुरक्षित रखा। केवल एक संन्यासी ही किसी भी प्रकार का वास्तविक लोक-संग्रह का कार्य कर सकता है, क्योंकि उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त है, और वह अपना पूरा-का-पूरा समय इसी ओर लगा देता है। एक ही सच्चा संन्यासी समस्त संसार का भाग्य बदल सकता है। यह शक्तिशाली शंकराचार्य ही थे, जिन्होंने केवल अद्वैत का सिद्धान्त स्थापित किया। वह अभी भी हमारे हृदय में निवास करते हैं।
परमहंस जन रोटी के कतिपय टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करते हैं और उसके बदले में द्वार-द्वार भटक कर वेदान्त, उपनिषदों, रामायण और भागवत के ज्ञान को भारत के
कोने-कोने तक पहुँचाते हैं। समस्त विश्व उनके प्रति ऋणी है। हम सबको उनका आभार मानना चाहिए। उनकी रचनाएँ अभी भी हमारा निर्देशन कर रही हैं। अवधूतगीता के कतिपय श्लोकों का अध्ययन करके देखें। आप तुरन्त स्वयं को दिव्य वैभव एवं महिमा की व्यापक ऊँचाइयों तक उन्नत हुआ अनुभव करेंगे। आप अपने-आपको एक परिवर्तित व्यक्ति पायेंगे। अवसाद, दुर्बलता, तनाव और व्याकुलताएँ सब तत्काल समाप्त हो जायेंगे।
जैसे विज्ञान, मनोविज्ञान, जीवविज्ञान और दर्शन-शास्त्र आदि विषयों में शोध-छात्र अथवा स्नातकोत्तर विद्यार्थी होते हैं, बिलकुल उसी प्रकार स्नातकोत्तर योगी एवं संन्यासी होने चाहिए जो अपना समय अध्ययन और ध्यान में लगाते हुए आत्म-तत्त्व की खोज करें। यह स्नातकोत्तर योगी जन विश्व को, धर्म के क्षेत्र में अपनी अनुभूतियाँ एवं उपलब्धियाँ प्रदान करेंगे। वे अन्य विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे और प्रचार हेतु विश्व में भेजेंगे।
यह गृहस्थियों का, जमींदारों का, राजाओं और महाराजाओं का दायित्व है कि वे इन संन्यासियों की देख-रेख करें और ये संन्यासी, बदले में उनकी आत्माओं की देख-रेख करेंगे। इस प्रकार संसार-चक्र भली-भाँति चलेगा। धरा पर शान्ति का साम्राज्य रहेगा।
प्रत्येक धर्म में ऐसे एकान्तवासियों के समूह हैं जो एकान्तपूर्ण एवं ध्यानमय जीवन व्यतीत करते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षु हैं, मुस्लिम धर्म में फ़कीर हैं, सूफी मत में सूफी फकीर हैं, ईसाई धर्म में फादर और 'रेवरेन्ड्स' (श्रद्धेय) हैं। यदि आप इन आश्रमों को अथवा संन्यासियों को अथवा जो त्यागमय एवं दिव्य साधनाओं से पूर्ण जीवन जी रहे हैं, उन सबको समाप्त कर देंगे तो धर्म की महिमा ही समाप्त हो जायेगी। यही लोग तो हैं, जो संसार के धर्मों को सुरक्षित रखे हुए हैं। यही लोग तो हैं जो गृहस्थियों को उस समय धैर्य एवं शान्ति प्रदान करते हैं, जब वे लोग कष्टों और मुसीबतों में होते हैं। यह सन्त दिव्य ज्ञान और शान्ति के अग्रदूत हैं। ये आत्मज्ञान के सन्देशवाहक हैं। आध्यात्मिक विज्ञान और उपनिषदों के रहस्यों के ये प्रचारक हैं। ये रोगियों के रोग का निवारण, असहायों को सहायता, निराशों को प्रसन्नता, निर्बलों को शक्ति तथा भयग्रसितों को साहस, वेदान्त के ज्ञान के द्वारा तथा 'तत्त्वमसि' महावाक्य के महत्त्व को स्पष्ट करने के द्वारा प्रदान करते हैं।
राजनैतिक स्वराज्य तो हमने प्राप्त कर लिया है; किन्तु क्या यह मानव को शाश्वत शान्ति एवं स्वतन्त्रता दे सकता है? क्या यह राजनैतिक स्वराज्य मानव के कष्टों और अज्ञान को पूर्णरूपेण समाप्त कर सकता है? क्या यह स्वराज्य जीवन की वास्तविक समस्याएँ हल कर सकता है? इससे मनुष्य को थोड़ी-सी अधिक सुख-सुविधाएँ मिल जायेंगी। वह और अधिक मक्खन, डबलरोटी और जैम खा सकेगा। किन्तु वह फिर भी दयनीय और दुःखी ही बना रहेगा, क्योंकि वह अभी भी अज्ञानग्रस्त ही है; उसे आत्मा सम्बन्धी ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर ही वास्तविक, शाश्वत और स्थायी सुख एवं आनन्द की उपलब्धि हो सकती है। केवल आत्म-स्वराज्य अथवा आत्म-साक्षात्कार ही मनुष्य को सच्ची स्वतन्त्रता एवं अमरत्व प्रदान कर सकता है। केवल आत्म-स्वराज्य ही उसे वास्तविक मुक्ति, अधिराज्य और परिपूर्ण सन्तुष्टि दे सकता है।
जो राजनैतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें भी गीता और उपनिषदों की भावना सहित जीवन जीना चाहिए। उन्हें नैतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व, नैतिक प्रशिक्षण, आत्म-त्याग, आत्म-संयम, आध्यात्मिक अनुशासन तथा अपने निजस्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहिए, उन्हें तीन प्रकार के तप-मन, वाणी और कर्म सम्बन्धी, जो भगवद्गीता में बताये गये हैं, उनका तथा पतंजलि महर्षि के यम और नियमों का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें आत्मा के अमरत्व, संसार की मायामय प्रकृति, आत्मा के ऐक्य और जीवन के ऐक्य के विषय में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उन्हें यह बात भलीभाँति समझनी चाहिए कि समस्त विश्व एक ही परिवार है, केवल तभी वह देश की और स्वयं अपनी सेवा, सच्चे अर्थों में कर सकते हैं।
१०२
कृष्ण, भगवान् नहीं है। वह अवतार नहीं है। वह एक कामुक ग्वाला था, जो गोपियों के संग रास रचाया करता था।
उस समय श्री कृष्ण भगवान् की क्या आयु थी भला ? क्या वे सातवर्षीय बालक नहीं थे? उस समय उनमें वासना की क्या झलक भी हो सकती है? रासलीला के रहस्य को, माधुर्य भाव को, भक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा को, आत्म-निवेदन अथवा भगवान् के प्रति पूर्ण समर्पण के रहस्य को कौन समझ सकता है? यह तो केवल नारद महर्षि, शुकदेव, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, हाफ़िज, रामानन्द जी और सखियाँ अथवा गोपियाँ ही थीं, जिन्होंने रासलीला के रहस्यों को समझा। सखियाँ ही केवल इसकी अधिकारिणी थीं। जब वे अभी बालक ही थे, क्या तब उन्होंने चमत्कार नहीं किये थे? क्या उन्होंने स्पष्टतः नहीं दिखा दिया था कि वे भगवान् हरि के अवतार ही हैं? शैशवावस्था में ही उन्होंने अपनी माता को विराट् रूप के दर्शन नहीं करवा दिये थे क्या ? कालिय नाग के फन पर खड़े हो कर क्या उन्होंने उसका वध नहीं किया? उन्होंने क्या स्वयं ही असंख्य कृष्ण रूप धारण नहीं कर लिये थे? गोपियाँ कौन थीं? क्या वह भक्तिभाव से मदोन्मत्त ऐसी दिव्यात्माएँ नहीं थीं जो सर्वत्र श्री कृष्ण को ही व्याप्त देखती थीं, जो स्वयं को भी कृष्णमयी ही देखती थीं? वंशी की ध्वनि ही उन्हें दिव्य आनन्दातिरेक की अवस्था में पहुँचा देती थी। वह देह-चेतना से अतीत थीं।
१०३
श्री राम एक साधारण मनुष्य हैं। वह भगवान् का अवतार नहीं हैं। वह अपनी पत्नी के वियोग में फूट-फूट कर रोये। इन्द्रजीत के बाण से आहत हो कर लक्ष्मण जब अचेत हो धराशायी हो गये थे, तब उनके रुदन से आकाश में दरार पड़ने जैसा हो गया था। यदि भगवान् थे तो राम अपने दिव्य स्वभाव को क्यों भूल गये ? सीता की अग्नि-परीक्षा के समय वह शोक-सागर में डूब गये थे। यदि वह अपना निजस्वरूप जानते थे, तो सीता-हरण पर इतने शोकातुर क्यों हुए ?
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्री राम वास्तव में परब्रह्म थे। वे कभी किसी बात से विचलित नहीं हुए, न ही उन्होंने यथार्थ में कुछ भी ऐसा किया था। वे कभी भी शोक या हर्ष से ग्रसित नहीं हुए; जन्म-मरण, सुख-दुःख से कभी प्रभावित नहीं हुए।
किन्तु आजीवन उन्होंने साधारण मनुष्य के समान व्यवहार किया। उन्हें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि रावण को यह वरदान प्राप्त था कि वह देव, असुर, राक्षस, यक्ष, सर्प, रीछ-भालू इत्यादि किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। रावण ने अभिमानवश मनुष्य को शक्तिहीन समझ कर इनमें उसका नाम सम्मिलित नहीं किया था, अतः उसका केवल मनुष्य द्वारा ही वध सम्भव था। इसलिए श्री राम को साधारण मनुष्य बन कर ही रहना था। नहीं तो, यदि श्री राम स्वयं का भगवद् स्वरूप प्रकट कर देते तो ब्रह्माजी के वरदान के अनुसार रावण का वध न कर पाते।
१०४
क्या दिवंगत आत्मा कोई भी मूर्त रूप धारण कर सकती है?
हाँ! किन्तु सभी आत्माओं में मूर्त रूप धारण करने की शक्ति नहीं होती, केवल वही उन्नत आत्माएँ मूर्त रूप धारण कर सकती हैं जो अतिभौतिक शक्ति से सम्पन्न हैं। वह मानव आकार धारण करती हैं, आत्मायन कुर्सी पर बैठती हैं और आत्मायन पर बैठे हुए के साथ हाथ मिलाती हैं। वह बातचीत भी करती हैं। उनका स्पर्श जीवित मानवशरीरधारी जैसा ही स्पृश्य और गर्म होता है। थोड़े ही समय के बाद आत्मा का हाथ अदृश्य हो जाता है। आत्माओं के चित्र भी उतारे (खींचे) गये हैं।
१०५
यह जानने की मेरी तीव्र इच्छा है, कि मेरे पति की आत्मा इस समय कहाँ है। मैं अति अनुगृहीत होऊँगी यदि आप मुझे बतायें कि मरणोपरान्त आत्मा का क्या होता है और दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, तथा हम देहधारियों को क्या वह देख अथवा सुन सकते हैं। प्रेतात्मवादी जो यह कहते हैं कि मृतात्माओं के साथ हम माध्यम (मीडियम) नामक साधन के द्वारा वार्तालाप कर सकते हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है ? क्या उससे उत्तर देने वाला वह मृतात्मा ही होता है?
प्रेतात्मवाद के, 'मीडियम' के और 'क्रिस्टल गेज़िंग' (स्फटिक में से देखना) इत्यादि के सम्मोहन में स्वयं को न फँसने दें। ये आपको भटका देंगे। मृतात्माओं के साथ सम्पर्क इत्यादि सब सनक है जिसका वास्तविक आध्यात्मिकता से कुछ सम्बन्ध नहीं है। जीवन का लक्ष्य इससे भिन्न है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने वास्तविक अनश्वर निज-आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करना। एकमात्र यह लक्ष्य प्राप्ति ही आपको परिपूर्ण आनन्द एवं शान्ति प्रदान करेगी।
आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा अस्तित्व के एक स्तर से दूसरे में प्रवेश होती है। मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म से पहले के बीच के समय में जीवात्मा अपने कर्मों के कुछ एक भाग का सूक्ष्मतर लोकों में भुगतान करती है। फिर निश्चित समय आने पर जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेती है।
दिवंगत आत्मा की सुनिश्चित शान्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है कीर्तन करना। अपने जप को बढ़ा दें, अन्य लोगों के कष्टों का निःस्वार्थ सेवा और दान द्वारा निवारण करें और हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करें।
अपने पति की दिवंगत आत्मा से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न न करें। दिवंगत आत्मा से सम्पर्क करने से, उनके उच्चतर आनन्दपूर्ण लोकों में गमन करने के ऊर्ध्वगामी पथ में आप बाधा खड़ी कर देंगी और उन्हें धरा-बन्धन में जकड़ देंगी। अपने पति को नीचे गिराने का प्रयास न करें। इससे उनकी शान्ति भंग होगी। 'मीडियम' को नियन्त्रित करने वाला प्रेत-नियन्त्रक अज्ञानी और धूर्त है। वह झूठ कहता है।
१०६
हमें अपनी सारी शक्तियाँ सामूहिक आर्थिक विकास की ओर लगा देनी चाहिए। यदि हम अपना समय आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने में, गीता अध्ययन और संकीर्तन में नष्ट न करें, प्रत्युत् उस शक्ति को उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्ति में लगायें, तो हमारी आर्थिक प्रगति शीघ्र होगी, उसके उपरान्त जो लोग चाहें वह दर्शन और धर्म की ओर प्रवृत्त हो जायें।
हमें अपनी भौतिक एवं शारीरिक शक्तियों को विकसित करके उन्नति के उसी शिखर पर, शक्ति और सुख-ऐश्वर्य के उसी स्तर पर पहुँच जाना चाहिए जिस पर पश्चिमी देश पहुँचे हुए हैं, न कि दर्शन शास्त्रों और ऐसी ही अन्य बातों में लगे रहें!
इस संसार 3/4 दो प्रकार के कार्यकर्ताओं-सामाजिक और धार्मिक की आवश्यकता है। सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य करेंगे। धार्मिक कार्यकर्ता आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार का विशेष कार्य करेंगे। एक बढ़ई का अपना कार्यक्षेत्र होता है और एक बिजली-मिस्त्री का अपना क्षेत्र है। आप बढ़ई को बिजली-मिस्त्री का और बिजली-मिस्त्री को बढ़ई का काम करने के लिए नहीं कह सकते। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और औद्योगिक विकास एवं रचनात्मक कार्य उनकी अपनी-अपनी दिशाओं में होना बहुत आवश्यक है। इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। किन्तु केवल धर्म ही लोगों की रक्षा कर सकता है। धर्म के अभाव में तो मनुष्य कहीं का भी नहीं रहता। यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले भी स्वयं को अनुशासित किये बिना, आध्यात्मिक आधार के बिना, धार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना तथा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का अभ्यास किये बिना एक अच्छे कार्यकर्ता नहीं बन सकते। नेता यदि स्वार्थी और भ्रष्टाचारी हों तो वह समाज को भ्रष्ट कर देंगे; क्योंकि वह अपने निजी अधिकार और पद के लिए ही लड़ते रहते हैं।
डबलरोटी, मक्खन, जैम और बढ़िया बिस्कुट आपको स्थायी शान्ति नहीं दे सकते। सुख-सुविधाएँ आध्यात्मिक जीवन और शान्ति के शत्रु हैं। ये व्यक्ति को नीचे गिरा देते हैं। अन्ततः व्यक्ति की इस धरा पर आवश्यकताएँ तो बहुत ही कम है। भगवान् का ध्यान तो आपको केवल मुसीबतों में ही आयेगा। आवश्यक तो आध्यात्मिक सम्पदा है, जो कि अक्षय है।
जिस कार्य से व्यक्ति का अज्ञान दूर होता है और उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, वहीं उसके कष्टों को दूर करके शाश्वत सुख प्रदान कर सकता है। और वह कार्य आध्यात्मिक प्रचार है। वह कार्य भक्ति और योग एवं वेदान्त के ज्ञान का प्रसारण है। यही मानव का सर्वोच्च कार्य है। यही सर्वोपरि यज्ञ अथवा योग है, समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ है।
केवल भारत के पास ही सर्वोपरि दिव्य सम्पदा है। विश्व के विभिन्न भागों के सर्वाधिक धनवान् लोग योग के अभ्यास के लिए, ऋषियों, सन्तों, योगियों एवं मनीषियों से निर्देशन प्राप्त करने के लिए तथा यह अनश्वर सम्पत्ति पाने के लिए हिमालय की ओर आते हैं।
धन से प्रसन्नता नहीं मिलती। पश्चिमी देशों के लोग इतना धन पा कर भी बिलकुल अशान्त हैं। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल आध्यात्मिक जीवन ही सच्ची शाश्वत शान्ति एवं प्रसन्नता दे सकता है।
१०७
योगी, अपनी यौगिक दृष्टि से भौतिक तत्त्वों के सूक्ष्म अंगों को कैसे देख लेता है ?
जैसे आप भौतिक पदार्थों को, आँखों के रूप में प्राप्त भौतिक उपकरण की सहायता से देखते हैं, उसी तरह योगी सूक्ष्मतर उपकरणों की सहायता से सूक्ष्म तत्त्वों को देखते हैं। जहाँ तक ज्ञान का सम्बन्ध है, अन्तर्ज्ञान के स्तर के अतिरिक्त अन्य सभी निम्न धरातलों पर दृष्टा और दृश्य के परस्पर सम्बन्ध का अस्तित्व है। केवल इतना है कि किसी वस्तु को देखने का कारण भी उसी से निर्मित होना चाहिए जिससे वह वस्तु बनी है।
योगी की दृष्टि को इससे और अधिक पूरी तरह से समझने के लिए आपको स्वयं योगी बनना चाहिए।
१०८
यदि सब-कुछ भगवान् द्वारा पूर्व-निर्धारित एवं पूर्व-नियोजित है, तो व्यक्ति कुछ भी करने अथवा न करने का प्रयास क्यों करता है? क्या किसी व्यक्ति को किसी काम में बार-बार असफलता प्राप्त होना भी भगवान् की इच्छा समझना चाहिए? क्या यह वास्तव में सत्य है कि हमें वही मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं अथवा ऐसा है कि हम जो चाहते हैं, वास्तव में उसके योग्य नहीं होते! मेरी सीमित बुद्धि में तो इस संशय का कोई स्पष्ट उत्तर समझ में नहीं आता। अतः आपकी महान् बुद्धि की ओर ही मैं अपना यह संशय भेजता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसे स्पष्ट कर भी देंगे।
यह सत्य है कि सब-कुछ भगवान् द्वारा पूर्व-निर्धारित और पूर्व-नियोजित है; और उनके पावन आदेशानुसार ही सब-कुछ घटता है। इसके साथ ही भगवान् ने प्रत्येक व्यक्ति को सही या गलत करने की, प्रेय-मार्ग और श्रेय-मार्ग में से विवेक से चयन करने की स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति भी दी है। यदि व्यक्ति सांसारिक सुख-भोगों की क्षणभंगुर और दुःखद होने की वास्तविक बुद्धि अथवा विवेक से सम्पन्न हो कर जागरूक रहता है तो वह सही दिशा में अपने प्रयास एवं परिश्रम से अपने प्रारब्ध को, अर्थात् उस जन्म में भोगने बाले पके हुए कर्मों के फल को बदल सकता है। भगवान् की विशेष अहैतुकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति अपना कुछ भी बना या बिगाड़ नहीं सकता। साक्षात्कार प्राप्ति तक के लिए भी भगवान् की कृपा का होना आवश्यक है। और कृपा प्राप्त करने के लिए गहन पुरुष प्रयत्न, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, जिसका योगवासिष्ठ में आद्यन्त वर्णन किया गया है, करना पड़ता है।
किसी भी किये जाने वाले कार्य की सफलता या असफलता, केवल भगवान् की कृपा के कारण से ही होती है। प्रत्येक परिणाम को वेदान्तिक उपेक्षा की दृष्टि से ग्रहण करें। मूक द्रष्टा बन कर भगवान् की लीला का आनन्द लें।
प्रत्येक व्यक्ति को वही मिलता है जिसका वह वस्तुतः पात्र होता है, कुछ भी न उसे उससे कम और न ही अधिक मिल सकता है। दैवी-सिद्धान्त, मनुष्य द्वारा बनाये गये कानूनों से बिलकुल भिन्न हैं। भगवान् का नियम, न्याय और निर्णय अन्तिम और असन्दिग्ध होता है। वहाँ रिश्वत का धन्धा नहीं चलता। उनका कानून मानव जाति के लिए, मानव जाति ही क्या सारी सृष्टि के लिए सदैव निष्पक्ष, एक-समान तथा सन्तुलित होता है। लौकिक इच्छाएँ केवल अहंकार की अभिव्यक्ति ही हैं, जो मनुष्य के मन, वाणी और कर्मों के द्वारा हर पल प्रकट होती रहती हैं। जैसे कि पहले भी कहा है, भगवान् की इच्छा के बिना इस पृथ्वी पर किसी भी मानव के द्वारा सांसारिक अथवा आध्यात्मिक कुछ भी प्राप्ति सम्भव नहीं है। भगवान् वास्तव में उसी की सहायता करते हैं, जो अपनी सहायता स्वयं करता है, और वह भी तब ही होता है, जब इच्छित वस्तु का प्राप्त होना उनके पावन-आदेशों के पूर्णतया अनुरूप लिखित हो। पालने से अर्थी तक, जन्म से मृत्यु तक, जागृति से अन्तिम सुषुप्ति के क्षण तक मनुष्य का निर्देशक तत्त्व होना चाहिए-परिणाम के चिन्तन से रहित, समर्पण पर आधारित स्वप्रयास, स्वप्रयास, स्वप्रयास और केवल स्वप्रयास ही।
१०९
यद्यपि गत इतने वर्षों से मैं सभी सत्संगों में भाग लेता रहा हूँ और भले ही पिछले इन सभी वर्षों से जप और ध्यान करता रहा हूँ तो भी अभी तक भगवान् और भगवन्नाम में मेरी सुदृढ़ श्रद्धा नहीं बनी है। अभी भी मेरे मन में परिवार, पद, धन और सांसारिक जीवन के प्रति मोह बना हुआ है। यह बड़ी विचित्र बात है स्वामी जी, इसे मैं स्वीकार करता हूँ! ऐसा क्यों ?
माया अत्यन्त शक्तिशाली है, केवल बहुत ही विलक्षण उदाहरण कोई-कोई हैं, जहाँ संस्कार अत्यन्त प्रबल होते हैं, नहीं तो व्यक्ति में ध्यान एवं चिन्तन से सम्पन्न जीवन के प्रति रुचि अपने-आपसे प्रकट नहीं होती। निस्सन्देह सत्संग, जप और ध्यान साधक को बहुत सहायता करते हैं; किन्तु अविद्या का आवरण इतना सघन है कि ये सब भी उसका छेदन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ये केवल संस्कारों की रचना कर देते हैं जो कि आगामी जन्मों में आकार ग्रहण करते हैं। हाँ, यदि आप इनके साथ-साथ विचार द्वारा विवेक विकसित करके वैराग्य उत्पन्न कर लेते हैं तो उन्नति अत्यन्त शीघ्र हो जाती है। वैराग्य और विवेक निश्चित रूप से आवश्यक हैं। इनके बिना कितना भी अधिक सत्संग, जप और ध्यान क्यों न किया जाये, तत्काल कोई परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा। माया अत्यधिक शक्तिशाली है, उसे केवल दृढ़ वैराग्य के द्वारा, केवल गहन वैराग्य द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है।
११०
स्वामी जी, काफी समय से ही मैं अपनी कक्षा की पुस्तकें पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही पुस्तक उठाता हूँ, मुझे लगता है कि यह पढ़ने योग्य नहीं है, क्योंकि मेरी क्षुधित आत्मा को सन्तुष्ट कर सकने वाला तत्त्व उनमें नहीं है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए संसार को त्यागने का यह समय अभी बहुत जल्दी है। इसके अतिरिक्त अभी तुम्हारे माता-पिता भी हैं। तुम्हें उनकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। ईमानदारी से अपनी रोज़ी कमाओ । परिश्रम करो। इसके साथ-साथ निमित्त भाव अपनाओ, अर्थात् स्वयं को भगवान् के हाथों का उपकरण समझने की भावना उत्पन्न करो। अपनी पढ़ाई करते रहो। यह निस्सन्देह सही है कि संसार सम्बन्धी ज्ञान मोक्ष नहीं देगा, फिर भी इसकी अपनी उपयोगिता है। कोई भी वस्तु अपने-आपमें दोषपूर्ण नहीं है, उस विषय सम्बन्धी ज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, यह महत्त्वपूर्ण है। अपनी व्यक्तिगत साधना को चलता रखने का प्रयत्न करो। मेरे बीस आध्यात्मिक नियमों का अपनी क्षमतानुसार पालन करो। आध्यात्मिक दैनन्दिनी (डायरी) को बनाये रखो। अपने जीवन के परम लक्ष्य को सदैव मन में रखो। उपयुक्त समय आने पर भगवान् स्वयं ही तुम्हें इस त्याग-पथ पर लगायेंगे।
१११
जीवन और ध्यान एक-दूसरे से मिश्रित कैसे हैं?
संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वभाव से दिव्य न हो। व्यक्ति में दिव्यता की मात्रा में ही अन्तर होता है, उसकी किस्म में नहीं। नास्तिक कहलाने वाले मनुष्य तक में दिव्यता की किरण होती है। कोई भी व्यक्ति सत्त्व, रजस् और तमस्, इन तीनों गुणों में से किसी भी एक से विहीन नहीं होता, मात्रा में ही अन्तर रहता है। व्यक्ति संशयवादी हो, निरीश्वरवादी अर्थात् नास्तिक हो, शून्यवादी हो अथवा और कुछ भी हो, उसमें जितना अंश सत्त्व का होता है, वह उसे कुछ-न-कुछ भले कार्य करने में सहायता करता है, जो उसे पुनः इसी प्रकार के भले कार्य करने में, इस जन्म में या अन्य आगामी जन्मों में प्रवृत्त कर देता है। रजस् और तमस् पूर्ण कर्म करते हुए भी वह अपने में विद्यमान सत्त्व की मात्रा के अनुसार सात्त्विक कर्म भी करता रहता है। इस जगत् में कोई भी व्यक्ति, भले ही वह डाकू हो, चोर हो, समुद्री डाकू हो या कोई अन्य, कभी भी केवल कुकर्म मात्र ही नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में दूषित एवं भले, दोनों प्रकार के कार्य अपने जीवन में करता है। अर्थात् जब तक वह प्रकृति के वश में है, वह दोनों प्रकार के मिश्रित कर्म करता है। जब भले कार्य करता है तो स्वाभाविक रूप से ही उसका मन दिव्यता की ओर, चाहे वह किंचित् मात्र सी ही हो, मुड़ जाता है, तो एक आन्तरिक प्रसन्नता उसे अनुभव होती है, भले ही वह इसका कारण समझ और बता न सके। ध्यान वस्तुतः सात्त्विक गुण है, जब जीवन उदात्त हो, तो उस क्षण मनुष्य निश्चित रूप से भगवान् का चिन्तन करता है।
इस सम्बन्ध में स्मरणीय बात यह है कि सात्त्विक कार्य भी पूजा या ध्यान के समान हैं। ध्यान का अर्थ, आवश्यक नहीं कि एकान्त कोने अथवा अलग कोने में बैठ कर भगवान् श्रीराम, श्रीकृष्ण, यीशु अथवा मोहम्मद के सम्बन्ध में चिन्तन करना या मानसिक अथवा बोल कर प्रार्थनाएँ करना ही समझा जाये। वह कार्य, जो व्यक्ति की स्थूलता को शुद्ध करने वाले हों, उन सभी को ध्यान माना जा सकता है। इसलिए सामान्य मनुष्य के सम्बन्ध में, जीवन-अमापनीय मात्रा में अज्ञान एवं ध्यान का मिश्रण है। यदि निश्चित रूप से किसी उन्नतात्मा गुरु के निर्देशनानुसार स्वेच्छापूर्वक ध्यान किया जाये तो व्यक्ति अकर्तृत्व एवं अभोक्तृत्व भाव सहित केवल भले और निष्काम कर्मों को ही करेगा, जिससे कि वह अपने जीवन को अधिक-से-अधिक प्रसन्नतापूर्ण, अधिक-से-अधिक ज्ञानपूर्ण तथा अधिक-से-अधिक आकर्षक अनुभव कर सके। यह दूसरी स्थिति, जो कि व्यक्ति का स्वैच्छिक पग बढ़ाना है, में वह विद्युत् वेग से अति शीघ्र उन्नत होता है जब कि पहली स्थिति में कछुए की सी धीमी गति से आगे बढ़ता है। इस प्रकार जीवन और ध्यान परस्पर मिले हुए हैं।
११२
आपका क्या विचार है कि आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य मध्यस्थ की भी आवश्यकता है?
हाँ, हाँ! वह है, इष्टदेवता। यह मन एकदम से अपने-आपसे अतीत नहीं जा सकता। अहंकार को समाप्त करना अत्यन्त दुष्कर है। आपकी चेतना को परम चैतन्य की अनुभूति कर सकना असम्भव सा ही हो जायेगा। इसलिए ध्यान करने के लिए इष्टदेव के नाम और रूप का चयन करना आवश्यक हो जाता है। समय आने पर यह इष्टदेव आपके समक्ष स्वयं को प्रकट कर देंगे और अहंभाव एवं मन को समाप्त करके आपको परम चैतन्य का साक्षात्कार करने की क्षमता प्रदान कर देंगे।
११३
स्वामी जी, मोक्ष प्राप्त करना क्यों आवश्यक है ?
इसे समझने के लिए आपको सत्संग और सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय करना चाहिए। सभी प्रकार की इच्छाओं एवं कुसंस्कारों से आच्छादित बुद्धि मोक्ष की आवश्यकता को समझ पाने के योग्य नहीं होती। ऐसी बुद्धि तो आसुरी बुद्धि होती है। गीता पढ़ें। सत्संग में भाग लें। सन्तों और संन्यासियों के प्रवचन सुनें। तब आपमें विवेक जाग्रत होगा। तब आप समझ सकेंगे कि यह संसार दुःख-दर्द से भरा हुआ है। तब फिर यह बंगला, यह मोटरगाड़ी, यह पद और यह वेतन जो सब आपका है, आपको और अधिक देर तक सन्तुष्ट नहीं कर पायेगा। आपकी आकांक्षाएँ उन्नत होंगी। आप स्वयं को मुक्त करना चाहेंगे। सूक्ष्मदर्शी लेंस तैयार करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है? अत्यधिक घिसाई करने के बाद ही उसमें से देखा जा सकता है। इसी प्रकार बहुत अधिक स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा ही आपकी बुद्धि इससे परे तक सोच पाने के योग्य हो पायेगी।
११४
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति इस जीवन से अतीत किसी भी प्रकार की आकांक्षा किये बिना एक भला जीवन जिये, सद्गुणों से सम्पन्न जीवन जिये, दानी, सत्य-परायण और उदात्त हो, समाज की भलाई के लिए कार्य करता रहे और एक अच्छा-नेक इंसान बन कर जीवन-लीला समाप्त कर ले ?
यदि आप भला जीवन जीते हुए मरना चाहते हैं तो आप एक भले व्यक्ति के रूप में मृत्यु को प्राप्त होंगे, सन्त के रूप में नहीं। आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।
आपने सैकड़ों भले व्यक्ति देखे हैं। किन्तु सन्त कितने देखे हैं? यहाँ तक कि आजकल तो सच्चे जिज्ञासु साधक ही दुर्लभ हैं। आप जो भले व्यक्ति कहते हैं, उन भले व्यक्तियों के भी बहुत से स्तर हैं। गाँधी जी जैसे भले व्यक्ति कितने हैं?
आपके यह भले आदमी क्या करते हैं? वे सत्य-परायण और नेक हो सकते हैं, वे दानशील और पवित्र भी हो सकते हैं; किन्तु अपने मन के भीतर कहीं गहराई में, इनके स्वार्थभाव छुपा रहता है। वे धन-संग्रह करेंगे और केवल अपनी पत्नी और सन्तान की चिन्ता करेंगे। क्या वे समस्त बच्चों को अपनी सन्तान जैसा समझेंगे? जब वे बाजार से मिठाई लाते हैं तब क्या दूसरों के बच्चों को पहले मिठाई देंगे? न, न! क्योंकि वे इस सत्य को नहीं जानते कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का वास है। जब तक यह सत्य, यह भाव उनके भीतर जाग्रत नहीं होता, जब तक वे इस परम सत्य पर ध्यान नहीं करते और इसका साक्षात्कार करने का प्रयास नहीं करते, तब तक त्याग और निःस्वार्थ सेवा का भाव कैसे विकसित कर सकते हैं?
मात्र पशु समान मनुष्य होने से, अवगुणों से पूर्ण आदमी होने से भला व्यक्ति होना निस्सन्देह अधिक अच्छा है। किन्तु यह एक लक्ष्य-विशेष का साधन मात्र है; यह लक्ष्य के निकटतर होने का एक पग मात्र है, यह अपने-आपमें एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं है। लक्ष्य तो आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको निश्चित रूप से भला बनना और भला करना होगा। और आपको इससे अधिक भी करना होगा- आपको विवेक, वैराग्य और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना होगा; जप और कीर्तन करना होगा, ध्यान करना होगा, सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय करना होगा। तब भगवान् की कृपा के द्वारा आप अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
११५
याज्ञवल्क्य महर्षि द्वारा प्रत्याहार प्राप्ति के लिए शरीर के १८ अंगों पर एकाग्रता करने की प्रविधि क्या है? कृपया विस्तार सहित बताइए।
महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा दी गयी एकाग्रता की प्रविधि में मन और प्राण को धीरे-धीरे से पाँव के अँगूठों से ले कर शरीर के एक-एक अंग पर, बहुत से गुह्य केन्द्रों में से होते हुए, ऊपर के अंगों की ओर बढ़ते जाना और वहाँ पर एकाग्रता एवं प्रत्याहार (हटा लेना) करते जा कर अन्ततः शिर की चोटी (शिखर) तक पहुँचने की श्रृंखला है। इस प्रकार इस प्रक्रिया के द्वारा मन और प्राण सारे शरीर से पूर्णतया खींच लिए जाते हैं, और अन्त में मस्तिष्क के केन्द्रीय स्थान में केन्द्रित हो जाते हैं जहाँ अभ्यासकर्ता गहन ध्यान में उतर जाता है।
याज्ञवल्क्य द्वारा बताये गये १८ अंग निम्नांकित हैं :
१. पाँव के अँगूठे, २. टखने, ३. पिण्डली, ४. पिण्डली से ऊपर, घुटने से नीचे तक की टाँग, ५. घुटने के मध्य, ६. जंघाओं का मध्य, ७. मलद्वार, ८. शरीर का मध्य भाग, कमर के नीचे का भाग, ९. जननांग, १०. नाभि, ११. हृदय, १२. कण्ठ का गड्डा, १३. तालू का मूल, १४. नासिका का मूल, १५. नेत्रगोलक, १६. भृकुटी का मध्यस्थल, १७. मस्तक, और १८. शिर का शीर्ष स्थल।
जब इन्द्रियाँ सक्रिय होती हैं, उसी समय मन बाह्यगामी होता है। अतः एकाग्रता अवरुद्ध हो जाती है। इन्द्रियों की सक्रियता प्राणों से होती है। प्राणों के प्रत्याहार से शरीर के विभिन्न अंग निष्क्रिय कर दिये जाते हैं और उनकी गति का निरोध कर दिया जाता है। यहाँ इस प्रक्रिया से, प्राणों का प्रत्याहार मन के प्रत्याहार से सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा प्राण और मन के अन्तर्सम्बन्ध के द्वारा यह इतने प्रभावशाली ढंग से नहीं होता। किसी अंग-विशेष पर जब गहन एकाग्रता के थोड़े से समय में मन को पूरी तरह से खींच लिया जाता है, तब अन्तर्गामी मन के साथ-साथ प्राणों का भी प्रत्याहार हो जाता है। प्राण भी मन का अनुसरण करते हैं।
इस प्रकार एक-एक अवस्था को पार करते हुए प्राणों का पाँवों के अँगूठों से ले कर तब तक प्रत्याहार होता जाता है जब तक वह अन्ततः शिर के शिखरतम केन्द्र पर नहीं पहुँच जाते और इस समय तक ध्याता को देह का भान विस्मृत हो जाता है, इस अवस्था में पहुँच जाने पर ध्यान निर्विघ्न आगे बढ़ता है तथा अत्यन्त प्रभावशाली हो जाता है।
यह निर्विघ्न गहन ध्यान में प्रवेश पाने की एक प्रक्रिया है। अपने ध्यान के आसन पर बैठ जायें। मनःस्थिति और भाव सही अवस्था में लाने के लिए थोड़ा प्रणव मन्त्र ॐ का उच्चारण करें। फिर इस समस्त व्यावहारिक जगत् को, इस पृथ्वी को भी नकार दें। जब आप उस अवस्था में पहुँच जायें जब आपको केवल अपनी देह का ही भान रह गया हो, तब प्रत्याहार की इस प्रक्रिया को आरम्भ करें। अपनी आँखें बन्द कर लें। पहले अपने पूरे मन को पैरों के अँगूठों पर ले जायें, वहाँ मन को एकाग्र करें। फिर धीरे-धीरे क्रमशः अँगूठों के क्षेत्र से आगामी बिन्दु पर ले चलें यथा टखनों पर, अब मन को यहाँ केन्द्रित करें। फिर वहाँ से आगे के बिन्दु पर ले जायें अर्थात् पिण्डली पर, यहाँ मन एकाग्र करें। फिर आगे के चार अंगों पर, और इसी प्रकार ऊपर की ओर बढ़ते जायें। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, आपकी रुचि और अभ्यास करने की गम्भीरता के अनुसार, आप इन समस्त १८ अंगों पर प्रत्याहार करते हुए ध्यान के मूल स्थान शीश के शिखर बिन्दु पर शीघ्र ही पहुँच कर ध्यान की वास्तविक अवस्था में पहुँच जायेंगे।
११६
स्वामी जी, मुझे लगता है कि मुझे महावाक्यों के अर्थ और उनका महत्त्व भलीभाँति समझ में नहीं आया है।
मैं आपको बतलाता हूँ। ध्यान से सुनें।
प्रथम वाक्य है, "प्रज्ञानं ब्रह्म-चैतन्य ब्रह्म है।" यह लक्षणा वाक्य है। गुरु अपने शिष्य को परिभाषा बताता है कि शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। फिर गुरु कहता है "तत् त्वम् असि । आप ही 'वह' हैं। आप सर्वत्र व्यापक शुद्ध चैतन्य हैं।" यह उपदेश वाक्य है।
फिर शिष्य अपने गुरु के बतलाये हुए विचार पर चिन्तन करता है, "अहं ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ।" यह अनुसन्धान वाक्य है।
अन्ततः, शिष्य को अनुभव हो जाता है कि वह आत्मा, जो उसके भीतर है वह ही ब्रह्म है : "अयमात्मा ब्रह्म। यह आत्मा ही ब्रह्म है।" यह अनुभव वाक्य है। क्या अब आपको स्पष्ट हो गया है?
११७
मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 'नौलि', 'उड्डियानबन्ध' तथा प्राणायाम का बहुत अधिक अभ्यास करने के कारण मेरे पेट की आँतों में अत्यधिक दर्द होने लगा है। यहाँ तक कि मुझे करवट से लेटना और साँस लेना भी कठिन हो रहा है। इतना सब होने पर भी मैं अपना योगाभ्यास और क्रियाएँ नियमित रूप से कर रहा हूँ। यदि यह किसी संकट का पूर्वाभास है तो कृपया तत्काल उत्तर दें। साथ ही फुफ्फुसों के दोनों ओर होने वाले असहनीय दर्द को दूर करने का भी कोई उपाय बतायें!
आपको इस समय जो असहनीय वेदना हो रही है, उसके कारण किसी भी प्रकार के भय की कोई आशंका नहीं है। तीन-चार दिन के लिए नौलि और उड्डियान करना बन्द कर दें। प्राणायाम आप निरन्तर करते रह सकते हैं, किन्तु भस्त्रिका जैसे प्राणायाम इन दिनों के लिए बन्द कर दें। थोड़ा-सा विश्राम ले लें। अति की ओर मत जायें। इस कथन को ध्यान में रखें, 'अति सर्वत्र वर्जयेत्।' किसी भी कार्य में 'अति' नहीं करनी चाहिए। मध्यम स्वर्ण पथ का अनुसरण करें।
जहाँ तक प्राणायाम का सम्बन्ध है, अभी आजकल सुखपूर्वक प्राणायाम तब तक ठीक रहेगा, जब तक आप पूरी तरह से अपने-आपको ठीक अनुभव नहीं करने लग जाते। अपने पेट के भीतरी अंगों को आराम देने से आप ठीक हो जायेंगे।
जब आपको लगे कि आप पूर्णतया ठीक हो गये हैं, तब सभी बन्ध, मुद्राएँ, क्रियाएँ और भस्त्रिका प्राणायाम आरम्भ कर दें। इस बात का ध्यान रखते हुए सदैव मध्यम पथ को अपनायें कि तीव्रता, अवांछनीयता और कठोर एवं उग्र अभ्यास द्वारा नहीं बल्कि सामान्य, सहज, गम्भीर एवं सतत प्रयास से ही आप वास्तविक उन्नति कर सकते हैं। हड़बड़ी और उग्र अभ्यास से पलक झपकते ही आनन्दमयी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा न समझें।
खुली हवा में सैर करें। सीधा, शवासन में लेट जायें। भगवान् से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने इष्टमन्त्र के जप से उनका आह्वान करें। पीड़ित अंगों (पसलियों) की, गर्म पानी में थोड़ी-सी तारपीन डाल कर सिकाई करें। थोड़ा पाउडर छिड़क दें। सिकाई करने के बाद थोड़ा तेल मलें। निश्चित रूप से आप ठीक हो जायेंगे।
११८
साधु और संन्यासी भिक्षा माँग कर क्यों खाते हैं ? क्या दान देने वाले के पाप कर्म और कुप्रवृत्तियाँ, उसके दिये गये भोजन में मिल कर साधु-संन्यासियों की मानसिक शान्ति को नष्ट नहीं कर देते ?
सच्चा और वास्तविक संन्यासी वह है, जिसे संसार के प्रति किंचित् भी मोहासक्ति नहीं है। ऐसे साधु एवं ब्रह्मनिष्ठ पुरुष तो अपनी आवश्यकताओं के प्रति भी उदासीन हीरहते हैं। उनको अपने लिए स्वयं भोजन बनाना भी नहीं चाहिए; क्योंकि स्वयं पकाने वाले व्यक्ति के मन में यह पकाना, वह पकाना अर्थात् सुस्वादु भोजन तैयार करने की इच्छा जाग्रत हो जाती है। इससे 'जिह्वा-चापल्य' उत्पन्न हो जाता है। साधना का उद्देश्य मन को नियन्त्रित करना है, जिसका सर्वोत्तम साधन है जिह्वा पर नियन्त्रण करना। इसीलिए साधु-संन्यासियों के लिए भोजन बनाने का निषेध किया गया है; अतः केवल पेट भरने तक के लिए भिक्षा-वृत्ति करने की अनुमति है। इसलिए भिक्षा माँगना साधु-संन्यासी के लिए पाप नहीं है।
भागवतों के जप, प्राणायाम, स्वाध्याय से उत्पन्न तप की अग्नि उन सब अपवित्रताओं को भस्म कर देती है जो अविकसित एवं कुभावनाग्रस्त लोगों द्वारा दिये गये भोजन से उत्पन्न हो सकती हैं।
११९
दार्शनिकों को पागल क्यों कहा जाता है? क्या दार्शनिकों में कुछ ऐसा है अथवा उन्हें यह कहने वालों में कुछ है?
सांसारिक व्यक्ति से तुलना करें तो दार्शनिक को इस दृष्टि से पागल कहते हैं कि वह बाह्य प्रकटीकृत रूपों में उस तरह से रुचि नहीं लेता, जैसे कि सामान्य लोग लेते हैं। दार्शनिक के लिए बाह्य जगत् केवल भ्रान्ति है, किन्तु सांसारिक व्यक्ति के लिए यह जगत् वास्तविक और शाश्वत है। इन दोनों में ही कोई भी पूरा गलत नहीं है, क्योंकि 'पागल' शब्द केवल परस्पर सापेक्षिक लक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है।
दार्शनिक जो कहता है, उसका साधारण मनुष्य विश्वास नहीं कर सकता और जो सामान्य व्यक्ति अनुभव करता है वैसा दार्शनिक नहीं कर सकता।
१२०
स्वामी जी, ब्रह्म में माया कैसे आयी ?
यह एक अतिप्रश्न है। आपके मन में यह प्रश्न विविध रूपों में आता है : कर्म कब से आरम्भ हुआ? जगत् की सृष्टि कब और कैसे हुई? संसार में बुराई क्यों है? वह अप्रकट स्वयं प्रकट क्यों हुआ? आदि आदि। ऐसा ही प्रश्न श्री राम जी ने योगवासिष्ठ में किया था और वसिष्ठ महर्षि ने कहा था, "तुम घोड़े के आगे गाड़ी को लगा रहे हो। इस प्रश्न को करने से तुम्हें कोई लाभ अथवा हल मिलने वाला नहीं है। ध्यान करो और ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त करो, तब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा। तब यह प्रश्न स्वयमेव ही समाप्त हो जायेगा।" कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। जब 'ज्ञान-प्राप्ति' हो जाती है तो प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। अतः इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं है।
ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, "लोकवत् तु लीलाकैवल्यम्।" यह केवल आपकी शंका को शान्त करने के लिए है। वास्तव में यह उत्तर नहीं है, क्योंकि उत्तर कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी, प्रत्येक जिज्ञासु के मन में शंका का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आप भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने विवेक का उपयोग करना होगा, संशय को शान्त करना होगा और फिर गहन साधना करके ध्यान के द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कार करना पड़ेगा। तब यह संशय और प्रश्न, सब समाप्त हो जायेंगे। एक बहुत बड़े ज्ञानी एवं योगी १२ वर्ष तक इस संशय में ग्रस्त रहे। फिर उन्होंने मुझे बताया, "अब चिन्ता समाप्त हो गयी है। इससे मैं १२ वर्षों तक परेशान रहा। मुझे कुछ भी उत्तर मिल ही नहीं रहा था। मैंने उसकी खोज में भागना बन्द कर दिया और ध्यान, जप एवं कीर्तन में लग गया। अब मुझे शान्ति और उन्नति-दोनों ही प्राप्त हो गयी हैं।" गुरु में श्रद्धा, ग्रन्थ साहिब में श्रद्धा, कीर्तन, जप, ध्यान और उचित पथ पर चलने का अभ्यास- ये सब आपको आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करने में सक्षम करके वहाँ पहुँचा देंगे, जहाँ संशयों और प्रश्नों की सम्भावना ही शेष नहीं रहती।
१२१
मैं यह बात भलीभाँति जानता हूँ कि सन्तोष से शान्ति मिलती है। किन्तु मुझे एक संशय है। यदि मैं सन्तुष्ट रहता हूँ, तो मेरी सभी अभिलाषाएँ मर जायेंगी। मैं अकर्मण्य और आलसी बन जाऊँगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही मैं इधर-उधर आता-जाता हूँ, परिश्रम करता हूँ और सक्रिय एवं उद्यमी रहता हूँ। कृपया मेरे इस संशय का निवारण करें। मैं बहुत किंकर्तव्यविमूढ़ हूँ।
सन्तोष आपको आलसी कभी नहीं बना सकता। यह सात्त्विक गुण है, जो व्यक्ति को ईश्वरोन्मुखी बनाता है। यह मन को शान्ति एवं शक्ति प्रदान करता है। यह अनावश्यक एवं स्वार्थपूर्ण परिश्रम को नियन्त्रित करता है। यह मनुष्य के आन्तरिक चक्षु को खोल कर उसके मन को दिव्य चिन्तन की ओर प्रेरित करते हुए सात्त्विक पथ की ओर अग्रसर करता है। यह उसकी स्थूल शक्ति, अर्थात् लोभ जो मनुष्य को स्वार्थपूर्ण परिश्रम में लगाने वाला है, को आध्यात्मिक शक्ति-ओज में रूपान्तरित कर देता है। जो मनुष्य सन्तुष्ट है, वह सत्त्व से पूर्ण भर जाता है और अब वह और भी अधिक कर्मठ हो जाता है। वह अन्तर्मुखी हो जाता है। वह अब आत्मस्थित हो आन्तरिक जीवन जीता है। वह अब सदैव शान्त है। वह प्रशान्त एवं एकाग्रचित्त हो कर अधिक उद्यमी हो जाता है। मन की समस्त बिखरी हुई किरणें अब संकेन्द्रित हो जाती हैं। क्या अब आप इस बात को समझ गये हैं?
यह सन्तोष की ही शक्ति है जिसके बलबूते पर साधु और संन्यासी, फकीर और भिक्षु, भिक्षा पर निर्वाह करते हुए, निश्चिन्ततापूर्वक संसारभर में भ्रमण करते रहते हैं। सन्तोष से शक्ति पा कर ही जिज्ञासु साधक आत्म-साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होता है और आध्यात्मिकता के दुष्कर एवं कंटकपूर्ण पथ पर निर्भीक हो कर चलने की वीरता रखता है।
१२२
जिन वस्तुओं से विज्ञान का सम्बन्ध है, उनके विषय में विज्ञान हमें सब-कुछ बताता है कि अमुक वस्तु कैसे बनती है और कैसे विकसित होती है। हमें विकास होने के चिह्न भी बता दिये जाते हैं। योग के अभ्यास में भी क्या साधक की उन्नति को माप सकने के इसी प्रकार के सुनिश्चित संकेत हैं? उदाहरण के लिए, कुछ ऐसे अनुभव हों जो उसे अमुक समय के बाद प्राप्त होंगे, जैसे तीन मास के अभ्यास के बाद होंगे या कुछ ऐसे अनुभव जो उसे एक वर्ष बाद अथवा और देर बाद होंगे ?
विभिन्न योगासनों से विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ प्राणायाम और हठयोग की क्रियाएँ क्रमिक श्रृंखलाबद्ध मानसिक अनुभव प्रदान करेंगी। सभी प्रकार के लोकोत्तर प्रकाश दिखायी देना और अनाहत नाद सुनायी देना इसी श्रेणी में आता है। जिन सन्तों ने इन योगों को दिया है, उन्होंने आध्यात्मिक अनुभवों के अत्यन्त सुनिश्चित स्तर दिये हैं। जैसे-जैसे कुण्डलिनी चक्र से चक्र की ओर बढ़ती जाती है, योगी को विशेष प्रकार के प्रमाणकारी अनुभव प्राप्त होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक चक्र का किसी एक विशेष तत्त्व पर शासन होता है और उस पर पूर्ण नियन्त्रण होता है, अतः वह उसी तत्त्व से सम्बन्धित अनुभव देता है।
इसी प्रकार तान्त्रिक साधना में भी है। उसमें भी आध्यात्मिक अनुभवों की सुनिश्चित सूची दे दी गयी है। प्रत्येक साधना की अपनी विशेष सिद्धि है; इस प्रकार जिस साधना का अभ्यास जो साधक करते हैं, उसे मापने वाले प्रमाणनीय अनुभव उन सभी को होते हैं।
किन्तु यह सभी अनुभव निम्न श्रेणी के एवं हल्के प्रकार के हैं। यह मानसिक अनुभव हैं, जो आवश्यक नहीं है कि साधक की आध्यात्मिक उन्नति को स्पष्टतया प्रकट करते हों। यहाँ तक कि भक्त के रोमांच एवं अश्रुप्रवाह के अनुभव भी, भले ही वह हठयोगाभ्यासी के अनुभव की श्रेणी में नहीं आते तो भी, यह भी आध्यात्मिक उन्नति के पूर्ण मानदण्ड नहीं हैं।
जब आप आत्मा के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं तो आप 'उस अनन्त' के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। योग अनन्त हैं और अनुभव भी अनन्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना योग है; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी संस्कार और वासनाएँ ले कर आया है और वह अपने निजी ढंग से लक्ष्य पर पहुँचने का प्रयास करता है। यह दोनों मिल कर उसे विभिन्न अनुभव प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही लोकातीत, अनन्त, शाश्वत आत्मा में प्रवेश करता है, साधक महान् आन्तरिक शान्ति एवं अवर्णनीय आनन्द अनुभव करता है। वह अपने आस-पास क्या हो रहा है, इससे जल्दी-जल्दी प्रभावित नहीं होता। इतना ही नहीं, अन्य जो भी उसके सम्पर्क में आते हैं, उनमें भी वह शान्ति एवं प्रसन्नता विकिरणित करने में सक्षम हो जाता है। वह भला बन कर भलाई प्रसारित करने लग जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का यह सर्वोत्तम संकेत अथवा मानदण्ड है। भगवान् परिपूर्ण भलाई हैं। इसलिए जो साधक भगवद्-साक्षात्कार की ओर उन्नत होता है, वह भलाई करने में उन्नत हो जाता है। उसके अवगुण अथवा दोष धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं और उनका स्थान उदात्त सद्गुण ले लेते हैं। यदि यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य उसमें उपलब्ध नहीं है तो अन्य सभी दृश्यावलोकन एवं ध्वनि-श्रवण इत्यादि पूर्णतया व्यर्थ हैं। अपनी उपस्थिति मात्र से ही योगी लोगों को भला जीवन जीने, घृणा से और दुर्भावना से मुक्त रहने के लिए प्रेरित कर देता है। उसका अपना हृदय समस्त विश्व के प्रति प्रेम से आपूरित है, अतः वह अत्यन्त स्वाभाविक रूप से तथा निःस्वार्थ भाव से सबकी सेवा तत्परतापूर्वक करता है। यह सभी वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति के संकेत हैं।
किन्तु इस सबसे परे, परम अनुभूति है। वह वर्णनातीत है। शान्ति एवं प्रसन्नता, मन की अबाध प्रशान्तावस्था-यह सब उन्नति के महान् संकेत हैं, किन्तु यह लक्ष्य-प्राप्ति नहीं है। लक्ष्य तो भगवान् के साथ एक हो जाना है। आपको निश्चित रूप से भगवान् के साथ एक होना चाहिए। स्वयं को सद्गुणों एवं भलाई में स्थापित कर लेने के उपरान्त 'ध्यान के सतत अभ्यास' द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वह परमानुभूति, जब योगी को यह अनुभव हो जाता है कि वह भगवान् के साथ एक हो गया है, इसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता।
१२३
श्री शंकराचार्य अद्वैती थे और उनके दार्शनिक लेख सिद्ध करते हैं कि वे नाम-रूप विहीन परब्रह्म में विश्वास करते थे, तो साकार ब्रह्म के प्रति उनका भक्तिभाव कैसे सम्भव था ?
क्योंकि ज्ञान और भक्ति, सार रूप में एक ही हैं! उनके द्वारा रचित विभिन्न स्तोत्रों को देखें। उनसे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उनमें अत्यन्त उच्च कोटि की भक्ति विकसित हो गयी थी। आत्म-निवेदन अथवा आत्म-समर्पण ज्ञान की ओर ले जाता है और ज्ञान एवं पराभक्ति परस्पर पर्यायवाची हैं।
आजकल लोग भक्ति की निन्दा करते हैं और वे सोचते हैं कि यह ज्ञान से निकृष्ट है। उन्हें भक्ति के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है। वे समझते हैं कि वे एकदम सीधे ही ज्ञान साधना में उतर सकते हैं। वास्तव में उन्हें भगवान् में श्रद्धा ही नहीं है। बस वे भगवान् के प्रति कहीं से कोई बौद्धिक धारणा प्राप्त कर लेते हैं, किन्तु यह अवधारणा उनकी कुछ भी सहायता नहीं करती। आवश्यक तैयारी के बिना ज्ञानयोग का कोई लाभ नहीं है।
१२४
स्वामी जी! कई स्थान, जैसे नागोर, शिरडी, तिरुवनमलै और ऋषिकेश, सदैव शान्ति से तथा एक विशेष प्रकार के आध्यात्मिक आनन्द से आपूरित हैं। क्या स्वामी जी, यह इसलिए है कि इन स्थानों में उन विशेष सन्त के व्यक्तित्व, उनकी तपस्या और सिद्धि का वहाँ के वातावरण की पावनता पर दीर्घ काल तक प्रभाव रहता है ?
हाँ, हाँ! और इतना ही नहीं; वह सन्त स्वयं भी अभी वहाँ उन स्थानों में निवास करते हों, यह भी सम्भव है। जीवन्मुक्त सन्त की यह स्वतन्त्र इच्छा है कि वह चाहे तो ब्रह्म में लीन हो जाये या सूक्ष्म रूप में रहते हुए लोक-संग्रह के कार्य, जिज्ञासुओं को निर्देशित करने, लोगों में धार्मिक उत्साह जाग्रत करने और इसी प्रकार के अन्य कार्य करने में लगे रहें। कई जीवन्मुक्त सन्तों में, परमात्मा की परम इच्छा के अनुसार ऐसा प्रकटीकरण हुआ है। अतः जिस स्थान पर सन्त ने तप किया और सिद्धावस्था प्राप्त की थी, उसी स्थान को उनकी अदृश्य आत्मा स्थायी रूप से निवास के लिए चुन ले तो वह स्थान सन्त के दिव्य गुणों-शान्ति, आनन्द एवं ज्ञान-विवेक का निवास स्थान बन जाता है।
१२५
इन्द्रियाँ सामान्यतया बहिर्मुखी हैं। कहते हैं कि यदि इन्हें अन्तर्मुखी कर लिया जाये, तो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेगा। 'अन्तर्मुखी करने' का क्या अर्थ है?
श्री राम के विषय में सोचें और राम, राम, राम का जप करें। जब आप मन में राम, राम कह रहे हों तो सामने श्री राम का चित्र रख लें। इन्द्रियाँ अन्तर्मुखी हो जायेंगी।
अभी तो आँखें पदार्थों की ओर दौड़ती हैं और कान विभिन्न आवाज़ों की ओर भागते हैं। जब आप ऊँचे स्वर में राम, राम बोलेंगे तो आपके कान केवल राम, राम सुनेंगे और इधर-उधर नहीं भागेंगे। आपके अन्तर्चक्षु केवल राम का चित्र देखेंगे। मन भगवान् पर एकाग्र हो जायेगा, यह विषय-वस्तुओं की ओर नहीं जायेगा। अतः अपने भीतर टकटकी लगा कर देखें, अन्तर्दर्शन करें। आप उस समय प्राणायाम भी कर सकते हैं। श्वास को रोक लें। प्राण ही इन्द्रियों को बल देते हैं। प्राणों को निरुद्ध कर दें और उन्हें संकेन्द्रित करने का प्रयत्न करें, जिससे कि इन्द्रियों को बाहर भागने की शक्ति न मिले। धीरे-धीरे, अभ्यास के द्वारा इन्द्रियाँ मन में लीन हो जायेंगी। मन एकाग्र हो जायेगा और आत्म-लीन हो जायेगा। यही समाधि-अवस्था है। नित्य इसका अभ्यास करें।
१२६
क्या पूर्णतया इच्छा रहित हो जाना सम्भव है ? पाश्चात्य दार्शनिकों का विचार है कि इच्छाओं का पूर्णरूप से त्याग असम्भव है।
पाश्चात्य दार्शनिक शिशु हैं। पतंजलि योग सूत्र में और योगवासिष्ठ में यह वर्णन किया गया है कि पूर्ण निष्कामता ही मोक्ष है। जीवन्मुक्त पूर्णरूपेण निष्काम होता है। इच्छा अपूर्णता का नाम है। जीवन्मुक्त परिपूर्ण आत्मा है। उसमें इच्छा कैसे हो सकती है? पूर्णता एवं अपूर्णता दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? अतः पूरी तरह इच्छा विहीन होना सम्भव है।
१२७
मनोवैज्ञानिक यह नहीं मानते कि परम चैतन्य-अवस्था भी कुछ है। वह तो केवल चेतन और अवचेतन को ही मानते हैं।
उल्लू कहता है, 'प्रकाश का अस्तित्व नहीं है।' तो क्या प्रकाश नहीं है? इसी तरह 'उल्लू' प्राध्यापक कहता है कि परम चैतन्यावस्था नाम की कोई वस्तु नहीं होती तो क्या परम चैतन्यावस्था समाप्त हो जायेगी? योगवासिष्ठ पढ़ें जो परम चैतन्य की सत्ता की पुष्टि करता है। जो परम चेतना को नकारता है, वह उस 'उल्लू' के समान है जो प्रकाश को केवल इसलिए नहीं मानता क्योंकि वह प्रकाश को देख नहीं सकता।
१२८
मैं दश मिनट से अधिक समय तक ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ समय के बाद मेरा मन विषय-वस्तुओं में भटकने लग जाता है।
जब आपकी रुचि जप और ध्यान में विकसित हो जायेगी, तब आप जप-ध्यान के लिए दीर्घ काल तक बैठ सकेंगे। जप और ध्यान को बढ़ाते जायें। रात्रि में सोने से पहले, प्रातः ४ बजे और दोपहर के भोजन से पहले भी आपको जप और ध्यान करना चाहिए। जैसे आप दिन में तीन-चार बार चाय पीते हैं, उसी तरह दिन में तीन-चार बार जप-ध्यान करना चाहिए। मन इधर-उधर भटकता है, तो भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अभ्यास करते रहने से यह धीरे-धीरे आपके नियन्त्रण में आ जायेगा। जब मन बहुत अधिक भागने लगे तो कीर्तन प्रारम्भ कर दें। कार्य करते समय और टहलते समय भी नाम-स्मरण- श्री राम, श्री राम करते रहें।
यदि लम्बे समय तक पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो आप सोफे पर बैठ कर जप और ध्यान कर सकते हैं। पद्मासन में ही बैठना है, यह आवश्यक नहीं है।
प्याज और लहसुन को पूर्णतया त्याग दें। इनका उपयोग पूरी तरह से छोड़ दें। घर में ही इन्हें बनाना बन्द कर दें। यदि आप इनका उपयोग घटाना आरम्भ करेंगे तो किसी एक दिन थोड़ा-सा खा लेंगे और फिर किसी दिन और अधिक खाने की इच्छा होने लगेगी। सिगरेट का आदी यदि इसे कम करने का प्रयत्न करता है तो कुछ दिन तक तो बहुत कम संख्या में पीता है, किन्तु फिर कुछ ही दिन बाद मानो पिछली कमी पूरी करनी हो, इस तरह से और भी अधिक धूम्रपान आरम्भ कर देता है। अतः इनको पूरी तरह से त्याग दें।
यदि आप अपनी गाय को बढ़िया बिनौले और खली खाने को देंगे तो वह पड़ोसी के खेत में घास खाने जाने के स्वभाव को छोड़ देगी। अभी आपका मन उन्हीं रसगुल्लों और पेड़ों के पीछे भागता है, जिनका स्वाद आपने उसे अब तक चखाया है। किन्तु यदि आप उसे जप और ध्यान के आनन्द को प्रदान करेंगे तो फिर यह सांसारिक विषय- वस्तुओं के पीछे नहीं जायेगा। जब आपमें जप और ध्यान के प्रति रुचि विकसित हो जायेगी तो यह अपने भटकने के स्वभाव को छोड़ देगा।
१२९
मैं कुछ असमंजस की सी स्थिति में इसलिए हूँ कि मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मुझे यह बताया गया है कि यदि मुझे यह ज्ञात हो जाये तो मेरे लिए ध्यान करना सरल हो जायेगा। क्या आप बता सकते हैं कि इसका समाधान कैसे खोजा जा सकता है?
जीवन का लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार है। यीशु के साथ एक हो जाना जीवन का लक्ष्य है। पाशविक वृत्तियों का रूपान्तरण करके दिव्यता को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। यदि आप क्रोध को नियन्त्रित कर लेते हैं, स्वार्थ भाव को दूर कर देते हैं और सहनशीलता, दया, निःस्वार्थता, उदारता, साहस, क्षमा की भावना को विकसित कर लेते हैं तो और दिव्य बन जायेंगे। क्या स्वार्थपरता अच्छी है? नहीं। अतः निःस्वार्थी बनें। क्या लोभी होना अच्छा है? क्रोध अच्छा है? काम-वासना अच्छी है ? कामुकता अच्छी है? दम्भाचरण अच्छा है? यह मानव को निम्न प्रवृत्तियों वाला बनाते हैं। अतः इन सबको दूर करके निःस्वार्थी, उदार, धैर्यशील, सहनशील, शुद्ध-पवित्र एवं विनम्र बनें। यह जीवन का लक्ष्य है।
१३०
क्या संन्यास लेना और अपने माता-पिता एवं अपने आश्रितों के प्रति कर्तव्य से विमुख हो जाना धर्म के विपरीत नहीं है? क्या व्यक्ति के परिवार के सदस्य वास्तव में उसके आश्रित होते हैं?
दूसरे लोग आप पर आश्रित हैं, यह धारणा केवल भ्रम के कारण है। केवल भगवान् ही प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखने वाले हैं। भ्रमवश आप यह समझते हैं कि अपने सगे-सम्बन्धियों की देख-रेख करने वाले आप हैं और उनके लिए आप अनन्त कष्ट-क्लेश तथा तकलीफें सहन करते हैं। यदि आप घर-गृहस्थी छोड़ कर एकान्तवासी भी हो जायें, तो भी भगवान् आपके परिवार के लिए सब व्यवस्था करके उनकी देख-रेख का अन्य प्रबन्ध कर देंगे और आपको कोई पाप नहीं लगेगा, किन्तु यह केवल तभी होगा यदि आपमें तीव्र एवं उत्कट वैराग्य है। स्वामी रामतीर्थ में ज्वलन्त वैराग्य था, अतः उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पत्नी एवं दो पुत्रों को छोड़ कर चले गये तथा संन्यास धारण कर लिया। इसी प्रकार भगवान् बुद्ध ने भी अपने राजसी वैभव और परिवार को त्याग दिया था और संन्यास धारण कर लिया था।
१३१
क्या कोई व्यक्ति इस संसार में वास्तव में दूसरों की सहायता कर सकता है, अथवा यह विचार उसके मन का भ्रम मात्र ही है? क्या सत्य यह नहीं है कि मनुष्य का विकास अथवा पतन उसके निजी कर्मों का फल होता है तथा दूसरे के कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ? क्या व्यक्ति की भली-बुरी परिस्थितियाँ उसके अपने ही कर्मों के परिणाम-स्वरूप ही नहीं होतीं? क्या कोई व्यक्ति आगे बढ़ कर उसकी और दूसरों की परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता है?
निश्चित रूप से व्यक्ति ऐसा करने में पहल कर सकता है। वह स्वयं अपना तथा दूसरों का भी भला कर सकता है। वह परिस्थितियाँ एवं वातावरण परिवर्तित कर सकता है। जरा देखिए, वह दूसरों के लिए कितना कर सकता है, सचमुच उनकी कितनी और कैसे सहायता कर सकता है। व्यक्ति अशिक्षितों एवं अज्ञानियों को शिक्षा और ज्ञान दे सकता। है, निर्धनों और जरूरतमन्दों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है।
वह अनाथों को शिक्षित कर सकता है तथा जहाँ असहाय बच्चों की देख-रेख की जाती हो, ऐसी संस्थाओं में सहयोग दे सकता है। व्यक्ति न केवल अपनी पूरी कमाई तक इसमें लगा सकता है, अपितु इससे भी अधिक बहुत कुछ किया जा सकता है। यथार्थ में दूसरों की सहायता कर सकने जैसे विचार के सम्बन्ध में आपको सन्देह क्यों है ? गाँधी जी का उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने राष्ट्र और विश्वभर के लिए क्या कुछ सेवा नहीं की!
१३२
भक्ति को विकसित करने का सबसे सरल ढंग क्या है?
भक्तिभाव को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक सरल मार्ग है-भगवान् की लीलाओं का बार-बार श्रवण करना। जितनी बार आप उनकी लीलाओं और महिमा को सुनेंगे, उतनी ही शीघ्र आपके मानस पटल पर उनका रूप अंकित हो जायेगा। और जब आप उनकी महिमा को सुनते ही रहेंगे तो भगवान् का चित्र आपके हृदय में सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट हो जायेगा। जैसे स्वर्णकार जिस मोम को धरती पर बिखरे हुए स्वर्ण-कण एकत्रित करने के लिए उपयोग में लाता है, उस पर प्रतिदिन स्वर्ण-कण चिपकते रहते हैं और जब वह पूरा भर जाता है तो वह भी स्वर्ण की भाँति चमकने लग जाता है। बिलकुल उसी तरह जब मन में भगवान् का रूप-आकार पूर्णतया सुदृढ़ एवं उज्ज्वल तथा सुस्पष्ट हो जायेगा तो भक्त में उनका अटूट स्मरण बना रहेगा और उत्कट भक्ति विकसित हो जायेगी।
१३३
क्या हम गुरु के निर्देशन के बिना कुण्डलिनीयोग का अभ्यास कर सकते हैं?
नहीं, उससे तो सब प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी। कुण्डलिनीयोग का अभ्यास करने के लिए आपके पास उस समय एक पारंगत शिक्षक का होना आवश्यक है।
किन्तु आप हठयोग के द्वारा कुण्डलिनी जाग्रत करने के लिए इतने चिन्तित क्यों हैं? सही ढंग से की जाने वाली किसी भी साधना से कुण्डलिनी जाग्रत हो जायेगी। यह भक्ति के द्वारा, गुरु-कृपा से, निष्काम कर्मयोग के सतत अभ्यास से, वेदान्त-विचार से और ध्यान से भी जाग्रत की जा सकती है। भगवान् के प्रति पूर्ण समर्पण कर देने और पूरी तरह से इच्छाविहीन हो जाने से आप हर प्रकार की अतीन्द्रिय शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। निःस्वार्थ सेवा सहित नाम-स्मरण इस युग के लिए सर्वोत्तम योग है। इससे आपको ईश-कृपा की प्राप्ति होगी और उनकी कृपा से, उनकी दिव्य शक्ति आपमें प्रवाहित होने लगेगी। उसके द्वारा आप क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते ? ये सभी अतीन्द्रिय शक्तियाँ आध्यात्मिक पथ की बाधाएँ हैं। हमें इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। यदि हम मानवता की सेवा में लगे रहें, इतना ही नहीं, यदि हम अनजाने में भी भक्तियोग या कर्मयोग के माध्यम से अतीन्द्रिय शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे तो उनके दुष्प्रभाव से ग्रसित हुए बिना हम अनजाने ही उन्हें मानवता की भलाई में उपयोग करते रहेंगे। यही ढंग सर्वोत्तम है।
१३४
स्वामी जी महाराज ! निर्गुण ब्रह्म के विषय में आपका क्या विचार है? क्या इसका अर्थ मात्र शून्य से है? फिर तो यह हमें कुछ प्रभावित नहीं करता। शून्यता अथवा 'कुछ भी नहीं' पर कौन ध्यान करना चाहेगा ?
निर्गुण 'कुछ भी न होना' नहीं है; अपितु यह तो प्रत्येक, जो अच्छा है, श्रेष्ठ है, उसका पूर्ण रूप में होना है। इसमें आपको पूर्ण शुभता, परिपूर्ण भलाई, समस्त सौन्दर्य, पूर्ण प्रसन्नता, स्वास्थ्य, मधुरता, शुद्धता, शान्ति, सब-कुछ अपनी परिपूर्णता में विकसित मिलेगी। दूर से यह परिपूर्णता अचिन्त्य अथवा अभावनीय हो जाती है और सन्तों ने इसे निर्गुण कहा। एक बार जब वे वहाँ पहुँच जाते हैं, तब वे इसकी अकथनीय अनुभूति में लीन हो जाते हैं। यह 'कुछ भी न होना' नहीं, अपितु सब-कुछ होना है, और यह इससे भी कहीं अधिक है, क्योंकि यह अनिर्वचनीय है, केवल इतना जान लें कि जो कुछ भी माया में दिखायी देता है, अथवा जो प्रतीत होता है, जैसे बुराई, कुरूपता, कष्ट, परिवर्तन, जन्म, क्षय, मृत्यु इत्यादि, यह सब इसमें नहीं हैं, क्योंकि यह माया से परे-मायातीत है।
निर्गुण ब्रह्म में कोई भी माया के गुण, यथा नीला रंग इत्यादि नहीं हैं। निर्गुण का अर्थ यही है।
१३५
स्वामी जी, भारतीय ग्रन्थों में 'काल' शब्द बहुत बार आता है। इसका सही अर्थ क्या है?
यह महाकाल का साकार रूप है। यह नाम-रूप को समाप्त करने वाला है। हमारे हिन्दू धर्म के सर्वेश्वरवादानुसार दिव्य-पदानुक्रम में बहुत से देवी-देवता हैं। जैसे हमार यहाँ सरकार में बहुत से मन्त्री और पदाधिकारी शासन को चलाने के लिए होते हैं, बिलकुल इसी तरह इस संसार को चलाने के लिए देवता हैं। जगत् की सृष्टि, पालन और संहार के विभिन्न कार्यों को निभाने के लिए अलग-अलग देवता हैं। कुछ को वायु, अप्रि और जल जैसे विभिन्न तत्त्वों का कार्यभार सौंपा गया है, कुछ जन्म, मृत्यु, जीवन-रक्षा और रोगों के प्रभारी हैं। काल अथवा यम या धर्मराज मृत्यु के देवता हैं। एक प्रकार से यह सारा संसार उनके अधीन अथवा उनके नियन्त्रण में है; क्योंकि जब समय आता है तो वह सभी प्राणियों के इस पृथ्वी के प्रवास-काल का अन्त कर देते हैं। केवल आत्मसाक्षात्कार-प्राप्त व्यक्ति ही इस काल का अतिक्रमण करता और निज-स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त करता है। सभी साधनाओं का उद्देश्य इस काल से अतीत जाना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना और कालातीत होना है।
१३६
कृपया मुझे बतायें कि वैश्व चेतना अथवा परम चेतना का क्या अर्थ है ?
यह चेतना की वह अवस्था है जिसमें आप जागरूक रहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है, सब परमात्मा है, और इसके अतिरिक्त वह ऐसा सूत्र है जो समस्त जीवात्माओं को परस्पर संयुक्त रखता है। भगवान् वह चैतन्य तत्त्व हैं जिससे सम्पूर्ण सृष्टि प्रकाशित होती है। इस परम चैतन्य अथवा भगवान् का साक्षात्कार प्राप्त करके व्यक्ति इस परिवर्तनशील जगत् के बन्धन से, नाम-रूपों की भ्रान्ति से मुक्त हो जाता है। यही परमात्म-साक्षात्कार अथवा आत्म-साक्षात्कार की अवस्था है।
आत्मानुभूति प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति पूर्णतया भगवान् में विलीन हो जाता है। यह ठीक इसी प्रकार से है जैसे नदियों का सागर में प्रवेश करना; वह अपनी अलग पहचान को खो देती है और अब आप इस अन्तर को नहीं जान पाते कि कौन-सा जल गंगा का है और कौन-सा गोदावरी का। भगवान् के अस्तित्व के समक्ष जगत् की भ्रान्ति उसी प्रकार मिट जाती है जैसे प्रकाश के आ जाने पर सर्प की भ्रान्ति रज्जु के अस्तित्व में सिमट कर समाप्त हो जाती है।
१३७
स्वामी जी, स्वयं को कर्म से मुक्त कैसे रखा जा सकता है ?
अपने दैनिक कर्तव्य-कर्म करते समय यह समझें कि जो कुछ भी आपके चारों ओर हो रहा है, यहाँ तक कि आपके अपने कर्मों के भी आप केवल द्रष्टा मात्र हैं। इसे साक्षी भाव कहते हैं। अपने अन्तर्मन में आपको अनुभव करना चाहिए कि आप अपने भीतर कार्य करने वाले से भिन्न हैं। यह वेदान्त का सिद्धान्त है।
इसके अतिरिक्त एक अन्य ढंग है जो इससे सरल किन्तु इतना ही शक्तिशाली है, वह है निमित्त भाव। अनुभव करें कि सभी कार्यों के वास्तविक कर्ता तो भगवान् हैं, आप उनके हाथों के एक उपकरण हैं। इस प्रकार समझ लेने से आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म भगवान् की पूजा बन जायेगा और आप उससे बंधेंगे नहीं। बिना किसी आशा और इच्छा के तथा अहंकार के बिना कार्य करें। कर्तापन की भावना का निर्मूलन कर दें, समझें कि कुछ भी करने वाला मैं नहीं हूँ। इस प्रकार आप कर्म-बन्धन की श्रृंखला से मुक्त रहेंगे। आप नये कर्म नहीं जोड़ेंगे। अपने प्रारब्ध कर्मों का भुगतान होते रहने दें, और इस प्रकार आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे।
१३८
स्वामी जी, अपनी सत्य की खोज में, मैं समझता हूँ कि भगवान् यीशु जैसे महान् रक्षक हमारी सहायता कर सकते हैं। किन्तु ऐसा तो नहीं होता कि ऐसे महात्मा सदा ही हमारे बीच विद्यमान रहते हों। फिर हम क्या करें, स्वामी जी ?
सन्त सदैव इस संसार में विद्यमान रहते हैं, दुर्जन भी सदा ही होते हैं। रक्षक और भक्षक-डाकू भी संसार में सदा ही रहते हैं, क्योंकि यह संसार द्वन्द्वात्मक है। यहाँ भले और बुरे-दोनों ही सदा विद्यमान हैं। परिपूर्ण भलाई तो केवल भगवान् में ही है। आपको सन्तों से निर्देश लेने चाहिए, केवल वही आपको ब्रह्मविद्या की शिक्षा दे सकते हैं। पुस्तकें निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगी, वह आपको महात्माओं से सम्पर्क स्थापित करवा देंगी। जब आप बाइबिल पढ़ते हैं, आपका भगवान् यीशु से सम्पर्क स्थापित हो जाता है। जब आप गीता पढ़ते हैं तो आपकी भगवान् श्रीकृष्ण के साथ समरसता स्थापित हो जाती है। इससे भी सहायता मिलती है। किन्तु जैसे पाकशास्त्र की पुस्तक पढ़ने मात्र से आप पाककला नहीं सीख सकते इसी तरह केवल पुस्तकें पढ़ कर आप योगासन भी नहीं सीख सकते। किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप अनन्त काल तक शिक्षक मिलने की प्रतीक्षा ही करते रहें, जब आपके मन में तीव्र इच्छा जाग्रत हो जाती है तभी आप अपनी रुचि अनुसार ग्रन्थ ले कर अभ्यास आरम्भ कर दें, उदाहरण के लिए बाइबिल जैसा कोई भी धर्मग्रन्थ ले सकते हैं।
१३९
क्या इन्द्रियाँ वंचित रखने के लिए अथवा नष्ट कर देने के लिए दी गयी हैं। संन्यासी, योगियों के आदर्श यही तो कहते हैं।
यूनानी आदर्श फिर भी जीवन के सुख-भोगों के सम्बन्ध में मध्यमार्गी विचारधारा रखते हैं। अधिकांश तर्कबुद्धिपरक पश्चिमी विचारक इसी को सही मानते हैं।
आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस पर बल देते हैं कि शरीर की माँगों अथवा आवश्यकताओं, जैसे भोजन और कामवासना, को मारने या दबाने से तथा अन्य मनोवेगों, जैसे मोह एवं आसक्ति को कुचलने से सामान्यतया लोग अपने लिए मानसिक समस्याएँ उत्पन्न कर लेते हैं। क्या इस धारणा में कुछ तथ्य है?
नहीं; इन्द्रियाँ हमें केवल वंचित रखने अथवा समाप्त कर देने के लिए नहीं दी गयी हैं। न ही सुख-भोगों में रत रहने के लिए दी गयी हैं। वास्तव में, किसी भी सांसारिक उद्देश्य के लिए इन्द्रियाँ नहीं दी गयीं। आध्यात्मिक साधकों के लिए सन्तों का सर्वोच्च दृष्टिकोण यही है। इन्द्रियाँ इसलिए दी गयी हैं कि इनका समझ-बूझ के साथ सतर्कतापूर्वक उपयोग करके उस वस्तु को प्राप्त किया जाये जो इन्द्रियों की पहुँच से कहीं अधिक ऊपर और परे है। आत्म-संयम के सही अभिप्राय और महत्त्व को समझने के लिए, इस प्रश्न को और अधिक व्यापक दृष्टिकोण से समझना होगा।
मनुष्य-जाति को इन इन्द्रियों के साथ-साथ श्रेष्ठ एवं दिशासूचक बुद्धि की योग्यता भी दी गयी है जिसके द्वारा भले-बुरे, उचित-अनुचित का विवेक एवं उनमें से चयन करने आदि की क्षमता भी उसे प्राप्त है। इन्द्रियाँ, इनके बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशन के अधीन रहते हुए कार्य करने के लिए मिली हैं; इसका उद्देश्य इन्द्रियों को पूर्ण रूप से नकारना नहीं, अपितु संयम के द्वारा एक ऐसा सुख प्राप्त करना है जो भोग-तृप्ति से प्राप्त सुख से लाखों गुणा श्रेष्ठ एवं उत्तम है। जब व्यक्ति इस तथ्य को अनुभव करता है, तो उसे समझ आ जाता है कि योग साधक के लिए किस प्रकार यह आत्म-संयम, कड़वाहट अथवा अरुचिपूर्ण अनैच्छिक दमन की बात बिलकुल भी नहीं है। सही समझ-बूझ के दृष्टिकोण से अपनाये जाने से यह प्रसन्नतापूर्ण एवं ऐच्छिक अनुशासन है जो अनन्त गुणा महान् एवं कहीं अधिक आनन्दपूर्ण अनुभव है। क्या मछली पकड़ने वाला, बड़ी मछली फँसाने के लिए लगाये जाने वाले कीड़े की हानि से कभी दुःखी होता है?
और फिर तपश्चर्या का मूलाधार अधिकांश लोग सही रूप में समझते भी नहीं। तपश्चर्या और त्याग दमन पर आधारित नहीं है। सही ढंग से की गयी तपश्चर्या के मूल आधार एवं सिद्धान्त ऊर्जा का संरक्षण एवं उदात्तीकरण हैं। सच्चा तपस्वी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रोक कर, दूसरी ओर मोड़ कर, उचित दिशा दे कर अन्ततोगत्वा उन्हें तत्त्वान्तरित कर देता है। बलपूर्वक किये जाने वाले दमन से होने वाले अनुचित अप्रत्यक्ष प्रभाव, यथा-मनोग्रन्थि, स्नायु-रोग इत्यादि का यहाँ स्थान ही नहीं है। निस्सन्देह, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के दमन सम्बन्धी विचार सही हैं, किन्तु व्यक्ति को यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि धार्मिक तपश्चर्या-जहाँ प्रक्रिया उचित दिशा में प्रवाहित करते हुए ऊर्जा का रूपान्तरण करने की है- वहाँ यह लागू नहीं होता; और इसका सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तपस्या उस योग का अंग है जो ऐसी अद्भुत पद्धति (मानसिक प्रशिक्षण एवं संस्कृति की) प्रदान करता है जिससे किसी भी प्रकार के स्नायविक रोग सम्बन्धी मनोग्रन्थियों अथवा सनकों की सम्भावना समाप्त हो जाती है।
सत्य तो यह है कि अधिकांश लोग यति-धर्म को सही ढंग से समझते नहीं, और दुर्भाग्यवश स्वयं संन्यासी ही इसे सही रूप में नहीं समझते जिसके परिणामस्वरूप, जिज्ञासु साधक-जगत् में हमें सच्चे अथवा वास्तविक तपस्वी बहुत ही कम मिलते हैं।
योग, आन्तरिक सुसंस्कृति, सामाजिक भलाई, आविष्कार, वैज्ञानिक उन्नति और अन्ततोगत्वा, अन्तर्दर्शन अथवा सहजानुभूति की प्राप्ति जैसे उच्चतर लक्ष्यों के लिए, संकेन्द्रित इन्द्रियों की अद्भुत क्षमताओं का समर्थन करता है। इन्द्रिय शक्तियों का रूपान्तरण बुद्धि एवं विवेकपूर्वक निर्णय के द्वारा किये गये संयम से किया जाना होता है। उच्चतर भले के लिए उनकी असीम क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए, न कि नासमझीपूर्ण, पशुवृत्तियुक्त क्षणिक सुख के लिए निर्लज्जतापूर्वक अपव्यय करते रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण से विचार करके, साधक को इन्द्रियों को क्षुधित रखने एवं नष्ट करने के लिए नहीं, अपितु वस्तुतः उन्हें सशक्त करने और अपने भले के लिए उपयोग करने को कहा गया है। इसके विपरीत, दुर्व्यसनिता अथवा अपव्यय वास्तव में इन्द्रियों के विनाश का कारण है।
यूनानी आदर्श, सामान्य मानव-जाति के लिए जीवन के सामान्य दर्शन के रूप में प्रतिपादित किया गया है। यति-धर्म, जैसा कि सन्तों द्वारा माना गया है, एक भिन्न अनुशासन है जो विशेष रूप से उस वर्ग के लिए है जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले, आत्म-साक्षात्कार के लक्ष्य के प्रति समर्पित साधक श्रेणी के लोग हैं। इस श्रेणी के लोग अत्यन्त भली-भाँति जानते हैं कि 'जीवन के थोड़ी मात्रा में सुख भोगने' का विचार केवल धारणा मात्र ही है और इसको वस्तुतः उपयोग में लाना असम्भव है। क्योंकि सुख भोगने की प्रवृत्ति स्वभावतः ही ऐसी होती है कि इन्द्रियों को जितनी बार भोग-रस लेने दिया जाता है उतनी ही और अधिक वेगवती होती जाती हैं। फिर यह उस व्यक्ति का स्वभाव बन कर उसे अपने पाश में जकड़ लेती है और उसको अधोगति के गर्त में गिरा देती है। सभी सन्तों का इस विषय में यही अनुभव है। अतः आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर साधकों के लिए किसी-न-किसी स्तर पर कठोर आत्म-संयम एवं अस्वीकरण अनिवार्य हो जाता है।
सांसारिक श्रेणी भले ही इसकी परवाह न करें, किन्तु साधक-वर्ग करता है। साधक-वर्ग एक विशेष उपलब्धि के लिए सुनिश्चित किया गया है। आप जानते हैं कि एक आधुनिकतम कलाबाज, एक बैले नर्तक अथवा एक कुशल मुक्केबाज़ अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण सफलता पाने हेतु स्वयं को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार स्वेच्छा से स्वयं को कठोर नियमों से अनुशासित रखता है। खेलों में विजेता होने के लिए प्रयत्नशील किसी भी प्रत्याशी को अपने प्रशिक्षण की अवधि के समय अपने पर स्वेच्छा से लगाये जाने वाले अस्वीकरण और अनुशासन की ओर देखें! उसकी तीव्र आकांक्षा एवं उत्साह उसके मन को प्रेरणा और प्रत्याशा के उच्च मनोभाव में रखते हैं। तब फिर क्या एक सच्चे यति में आध्यात्मिक पथ में अनन्त एवं महानतम उपलब्धि हेतु इस आध्यात्मिक प्रशिक्षण अवधि में ऐसी आकांक्षा एवं अभिरुचि नहीं होनी चाहिए?
१४०
अपच को कैसे दूर किया जा सकता है?
जब आपको भूख लगे तब ही भोजन करें। भोजन के बाद आगामी भोजन लेने के बीच के समय में कुछ न खायें। शान्त मन से धीरे-धीरे खायें। भलीभाँति चबा कर खायें। बहुत प्रकार के व्यंजन एक समय के भोजन में न लें। भोजन से एक घण्टा पहले अथवा एक घण्टे बाद पानी का गिलास पियें, भोजन के साथ कभी भी पानी न लें। एकादशी को उपवास करें। प्रातः ९ बजे से पहले और सायं ७ बजे के बाद कुछ भी न खायें। अपने दाँतों का ध्यान रखें। भोजन के तुरन्त पहले या बाद में किसी भी प्रकार की मानसिक अथवा शारीरिक थकान से दूर रहें। कम-से-कम आधा घण्टा आराम करें। तीव्र गति से की जाने वाली लम्बी सैर लाभदायक है। पश्चिमोत्तान आसन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मयूरासन-ये सभी योगासन अपच को दूर करते हैं। मानसिक अवसाद और तनाव इत्यादि भी पाचन क्रिया पर प्रभाव डालते हैं, अतः सदा प्रसन्नचित्त रहें। नियमित रूप से जप करते रहें।
१४१
बढ़ी हुई काम-वासना को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है?
काम-वासना मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस वृत्ति को रोकने का सर्वश्रेष्ठ साधन कठोर एवं गहन वैराग्य का विकास है। धार्मिक पुस्तकों के स्वाध्याय से, महात्माओं के साथ निरन्तर सत्संग से, 'मैं कौन हूँ?' इस विचार द्वारा आत्म-निरीक्षण से, संसार को सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए विवेकपूर्वक विचार करने से तथा अतिभोग से उत्पन्न होने वाले रोगों एवं आध्यात्मिक अवनति को जान लेने से ऐसे वैराग्य को विकसित किया जा सकता है। गीता में भगवान् द्वारा कहे गये इन वचनों का स्मरण बनाये रखें।
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।।
(१६/२१)
मेरी पुस्तक 'योग आसनाज़' तथा 'साइंस ऑफ़ प्राणायाम' में वर्णित आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। आत्म-विस्मृति की अवस्था तक पहुँच जाने पर्यन्त कठोर जप करें। समस्त नारी-जाति को भगवती देवी माँ, पूज्य मातृ शक्ति का प्रकटीकृत रूप समझते हुए व्यवहार करें। अपने से विपरीत लिंग के प्रति मातृ भाव बनाये रखें। महिलाओं के चेहरे की ओर देखना छोड़ दें, केवल उनके पैरों की ओर ही दृष्टि रखें जिससे मन में कुभावना का अथवा अनुचित संकेत करने का भाव ही उदय न होने पाये। सदा शीतल जल से स्नान करें। जिह्वा पर संयम रखें। जिह्वा को ढील देने का अर्थ है व्यक्ति को संकट में डालने वाली कामुकता को बुलावा देना। स्वयं को सदैव पवित्र एवं उदात्त विचारों में व्यस्त रखें। हनुमान्, रामदास इत्यादि के जीवनचरितों के स्वाध्याय से ब्रह्मचर्य की महिमा को जानें। मेरी पुस्तक 'हाओ टू गेट वैराग्य' में वर्णित नियमों के अनुसार अपना निरीक्षण करें। आवश्यकताओं और इच्छाओं को कम करें। जितनी अपनी 'मैं' को घटाते जायेंगे उतने ही नकारात्मक भाव समाप्त होते जायेंगे।
१४२
गोहत्या के सम्बन्ध में आपकी विचारधारा क्या है ? क्या आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि इसी के कारण हमारे राष्ट्र की अवनति हो रही है?
धर्मग्रन्थ, मान्य व्यक्ति और धर्मग्रन्थों की कथाएँ उतनी ही सत्य हैं जितने स्वयं भगवान्। ये सभी निश्चित रूप से एवं निस्सन्देह कहते तथा उद्घोषित करते हैं कि हिन्दू धर्म के विश्वासानुसार जो तैंतीत करोड़ देवता हैं उन सबका उसी प्रकार गोमाता की देह में भी निवास है जैसे कि पवित्र तुलसी के पौधे में है। हमारे धर्मग्रन्थों में अत्यन्त निर्भीकता सहित घोषित किया गया है कि गाय एक ऐसा जीव है जिसे मनुष्य के देहान्त के समय उसकी आत्मा की सद्गति हेतु दान किया जाना चाहिए। निश्चित्त रूप से गाय पूजनीय है। पंचगव्य (गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर) को ऋषि पंचमी इत्यादि जैसे कई व्रतों में प्रायश्चित्त के रूप में लेने के लिए कहा गया है। गाय की पवित्रता के सम्बन्ध में कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। गोपूजा उतनी ही लाभकारी है जितनी संन्यासी (साधु) पूजा। यदि अधिक नहीं तो यह सकल देवता पूजा के तुल्य तो है ही। जब ऐसा है तो निश्चित रूप से गो-वध अत्यन्त निन्दाजनक है।
१४३
हमारे पुराणों में यह बताया गया है कि प्राचीन युग में हमारे पूर्वजों को प्रायः आकाशवाणी सुनायी दिया करती थी जिसके द्वारा उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत करा दिया जाता था। क्या यह विश्वास करने योग्य है? अथवा, क्या यह उनकी आन्तरिक सहजबुद्धि ही होती थी ?
चारों युगों में एक नियम रहा है। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जाता है, मानव की चेतना स्थूल से स्थूलतर होती जाती है। गत युगों में मनुष्य की चेतना-शक्ति इस युग की अपेक्षा सूक्ष्म थी।
सत्य युग में भगवान् मानव जाति के मध्य में विचरण किया करते थे। मानवीय चेतना तब दिव्य चेतना से दूर नहीं हुई थी। त्रेता युग में मनुष्य की चेतना स्थूलतर हो गयी। तब यद्यपि भगवान् की निरन्तर मानव जाति के मध्य उपस्थिति नहीं रही, किन्तु भगवान् के अवतार प्रायः होते रहते थे। द्वापर युग में मनुष्य की चेतना शक्ति और अधिक स्थूल हो गयी; और केवल नारद, विश्वामित्र इत्यादि के समान ब्रह्म ऋषि और आकाशवाणियों द्वारा भी लोगों को भावी आशंकाओं के प्रति सूचित किया जाने लगा।
अब हमें लगता है कि आकाशवाणी अत्यन्त दुर्लभ और विलक्षण वस्तु है, प्राचीन युगों में ऐसा नहीं था। देवता भी मनुष्यों के मध्य विचरण किया करते थे और आकाशवाणी लोगों को प्रायः पूर्वाभास दिया करती थी। जैसे हमारी सरकार है, बिलकुल उसी प्रकार देवताओं की भी अपनी सरकार है। जब भी वे मानव जाति को कोई सूचना देना चाहते थे, आकाशवाणी के माध्यम से दे देते थे।
आजकल देवता अधिकांश रूप में स्वप्नों और दर्शनाभास द्वारा सन्देश देते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से इस युग में सन्देश देने का केवल यही साधन शेष रहा है।
१४४
यह एक सामान्य शिकायत है कि स्वामी जी महाराज, जिनसे कि जाति, धर्म और लिंग इत्यादि सभी से ऊपर होने की आशा की जाती है, को प्रायः महिला अतिथियों से घिरे हुए पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें, यही प्रार्थना है।
मैं पुरुषों को अपने निकट बैठने से रोकता नहीं हूँ। वास्तव में कार्यालय में सदा ही बहुत से पुरुष मुझे निकट से घेरे रहते हैं। वे दर्शनार्थियों के लिए रखे गये बैंचों पर बैठते हैं, और महिलाएँ स्वाभाविक रूप से भारतीय परम्परा को ध्यान में रखते हुए आगे धरती पर, मेरी मेज़ के आस-पास बैठ जाती हैं। चलते समय पश्चिमी सभ्यता की भाँति और पुरुष वर्ग अपनी ही इच्छा से स्त्रियों को आगे चलने देते हैं। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे महिलाएँ ही मुझे चारों ओर से घेरे रहती हों।
यह सब तो बता दिया, किन्तु इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि महिलाओं में पुरुषों से अधिक भक्ति होती है जब कि पुरुषों में बुद्धि-तत्त्व की प्रधानता रहती है। महिलाओं का भक्तिभाव ही उन्हें कार्यालय में मेरी मेज़ के निकट बैठा देता है, और पुरुषों की बुद्धि उनसे इसके औचित्य का प्रश्न करवाती है! जब बुद्धि-प्रधान पुरुष में भक्ति का भी विकास हो जाता है, तब उसके परिणामस्वरूप समझदार मन और उदार दृष्टिकोण की प्राप्ति हो जाती है, जो शीघ्र ही आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं।
मैं महिलाओं की भी उतनी ही आध्यात्मिक भलाई चाहता हूँ जितनी पुरुषों की; सम्भवतया साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिए मैं महिलाओं को निर्देश देने में थोड़ी अधिक रुचि लेता हूँ। इसके तीन कारण हैं। प्रथम तो यह कि इस कथन से आप भी परिचित हैं कि, “जो हाथ पालना झुलाते हैं, वह संसार पर शासन करते हैं।" नारी, पुरुष को आकार देती है, यदि वह आध्यात्मिक है, तो निस्सन्देह समस्त मानव जाति पवित्र और शान्तिपूर्ण होगी। दूसरा पुरुष जब छायाओं के पीछे भागने में, धन-अर्जित करने और संसार के निःसार वस्तु-पदार्थों को एकत्रित करने में व्यस्त रहते हैं, तब यह नारियाँ ही हैं जो अपनी सामर्थ्य अनुसार धर्म का संरक्षण करती हैं। हम जितनी भी दे सकें, उतनी उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और प्रेरणा देनी चाहिए। तीसरा पुरुष की अर्धांगिनी होने के नाते यदि नारी आध्यात्मिक रुचि सम्पन्न होगी, तो मैं जानता हूँ कि वह अपने पति को पीछे नहीं रहने देगी। वह पुरुष की सहधर्मिणी है और यदि सांसारिक कामों में व्यस्त पुरुष थोड़ी देर के लिए अपनी भूमिका को विस्मृत भी कर देगा तो भी वह ऐसा नहीं करेगी और धैर्यपूर्वक प्रयत्न करती रहेगी तथा अन्ततः उसे भी दिव्य जीवन जीने में लगा लेगी।
१४५
स्वामी जी, आप तो सन्तत्व को सदैव विनम्रता के साथ संयुक्त किया करते हैं, फिर आपको अपनी फोटो उतरवाने में इतनी रुचि क्यों है ?
चाक्षुष शिक्षा पद्धति के पीछे निहित शक्ति, जिसे आजकल मनोवैज्ञानिक पुस्तकीय शिक्षा से अत्यधिक उत्तम मानते हैं, उसका स्पष्टीकरण आपको तब हो जायेगा, जब आप एक सामान्य तथ्य पर विचार करके देखेंगे। आप अपनी पढ़ाई की मेज पर थोड़ी सी अच्छी किताबें, कुछ चित्रकथाएँ और कुछेक चित्र रख दें। अपने बच्चों और मित्रों को पढ़ने के लिए कमरे में बुलायें। सबसे पहले वे क्या उठाते हैं, इसे देखें, पुस्तकें ? नहीं! सबसे पहले चित्र और उसके बाद चित्रकथाएँ।
दक्षिण भारत में वृद्ध माताएँ अपने नाती-पौत्रों को चित्र उतरवाने से अकारण ही यह कहते हुए नहीं रोकर्ती कि, "चित्र उतरवाने से तुम्हारा ओज चला जायेगा।" यह सच है कि आपकी कान्ति आपके चित्र में चली जाती है। आपके मित्रों और सम्बन्धियों के लिए, आपके नज़दीकियों और प्रियजनों के लिए आपका चित्र सजीव है, आपकी आभा सहित जीवन्त है। इसलिए भक्त के लिए भगवान् का चित्र, शिष्य के लिए गुरु का चित्र उनकी जीवन्त उपस्थिति होती है। ध्यान के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
आप पूछेंगे कि फिर इतने अधिक चित्र क्यों ? वह इसलिए कि अलग-अलग लोग, अलग-अलग तरह के चित्र चाहते हैं। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में, अलग तरह की पृष्ठभूमि में चाहते हैं। मुझे सभी को सन्तुष्ट करना पड़ता है। बीस वर्ष पहले लिया गया मेरा चित्र, आज के लिये गये चित्र से चित्रकला की दृष्टि से, युवावस्था के कारण अधिक अच्छा हो सकता है, किन्तु जो साधक मुझे आज प्रथम बार देख रहा है वह यही चाहता है कि जैसा मैं आज हूँ उसे वैसा ही चित्र चाहिए बीस वर्ष पहले वाला नहीं, भले ही वह कितना भी अच्छा हो! और फिर लोग अपने साथ मेरा चित्र लेना चाहते हैं, यह चित्र उनके लिए आश्रम आने के स्मारक चित्रों का कार्य करते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं।
चित्र उतरवाने के लिए इनकार करना, सूक्ष्म अहंकार का परिचायक है। यह विनम्रता की ओट में भीरुता अथवा आलोचना का भय है। यदि आपमें सही विवेकशीलता है तो इस बात को आप तुरन्त समझ जायेंगे।
१४६
आप जैसे महान् सन्त, जिन्होंने सब-कुछ त्याग दिया है, क्या उन्हें शीतकाल में ओवरकोट पहनना चाहिए?
सन्त या संन्यासी काँटों पर तो नहीं सोयेगा, मिट्टी-पत्थर तो नहीं खायेगा, सिर के बल नहीं चलेगा और न ही दीवारों में सिर फोड़ेगा। उसके शरीर को भी भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी इत्यादि लगती है और बड़ा कोट केवल एक टुकड़ों में काट कर, सुविधाजनक बनाने के लिए जिससे कि शरीर ठीक से ढका जा सके, ऐसा सीधा खड़ा सिल दिया गया कम्बल ही तो है, जिससे कि सेवा करने के लिए बाँहों की गतिविधियों में बाधा न आये ! कम्बल एक लम्बाई में टुकड़ा है। मैं कोट को अधिक महत्त्व नहीं देता।
अन्ततः आपको बाह्य पोशाक-पहरावे की ओर क्यों इतना ध्यान देना आवश्यक है? मनुष्य के भीतरी व्यक्तित्व को, उनके विचारों, भावों और गुणों को देखने का प्रयास करें, बाहरी विवरण को नहीं। केवल एक सच्चा सन्त ही दूसरे सन्त को समझ सकता है।
देह पर भस्म रमा कर, लम्बी दाढ़ी या जटाएँ रख कर कोई सन्त नहीं बन जाता। मेरे इस लम्बे कोट को आप क्यों इतना महत्त्व दे रहे हैं? विलासिता अथवा ठाट-बाट की दृष्टि से पहनावे में रुचि रखना निस्सन्देह अनुचित है, किन्तु केवल आवश्यकतापूर्ति के उद्देश्य से शरीर को निश्चित रूप से उचित पोशाक और भोजन देना आवश्यक है।
१४७
आप प्रसिद्धि पाने के इतने इच्छुक क्यों हैं? आप निःस्वार्थ सेवा के सम्बन्ध में इतनी बात करते हैं और फिर भी हम देखते हैं कि आप नाम-यश के लिए इतना कार्य कर रहे हैं!
पहली बात तो यह है कि मैं नाम-यश के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति निःस्वार्थ सेवा करता है तो उसके न चाहने पर भी उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। महात्मा गाँधी के जीवन में भी ऐसा होते आपने देखा है। केवल निःस्वार्थी व्यक्ति ही जानते हैं कि वह अपनी इस प्रसिद्धि का उपयोग और अधिक लोगों के लिए, और अधिक सेवा में कैसे कर सकते हैं।
दूसरी बात, इस प्रसिद्धि के माध्यम से ही मैं अधिक-से-अधिक जिज्ञासु साधकों के सम्पर्क में आ सकता हूँ। यह प्रसिद्धि मुझे अधिक-से-अधिक लोगों की सेवा कर सकने का सुअवसर प्रदान करती है। और लोग जब मुझे महिमान्वित करते हैं तो वह केवल संन्यास को, केवल साधनामय दिव्य जीवन को ही महिमान्वित करते हैं, और अन्य लोगों की दृष्टि में यह बात आ जाने से, वह सब भी दिव्य जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, साधना करने की, आत्म-साक्षात्कार पाने की और साधना की उपेक्षा न करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि महापुरुषों का जीवन हमें स्मरण कराता है कि हम भी अपने जीवन को उदात्त बना सकते हैं।
तीसरी बात, जो व्यक्ति नाम-यश के पीछे भागने वाला होता है, वह छोटे-मोटे सेवा-कार्यों में नहीं लगता, वह प्रत्येक के साथ घुल-मिल कर बात नहीं करता, वह चुटकुले सुना कर लोगों को अपनी उपस्थिति में ही हँसने नहीं देता; सर्व-साधारण लोगों के बीच वह स्वयं को अलग और ऊपर रखता हुआ अपने प्रति सबमें अपनी विलक्षणता और सम्मान का भाव बना कर रखता है और अपनी बातचीत में बनावटी उच्च दार्शनिक विषयों पर ही स्थिर रहते हुए सबमें अपना प्रभाव बनाये रखने का प्रयत्न करेगा और स्वयं को सबसे ऊँचा दिखाने में प्रयत्नशील रहेगा। मैं तो सबके साथ घुल-मिल कर रहना चाहता हूँ और सबको ऐसा अनुभव होने देना चाहता हूँ कि मैं भी उनमें से ही एक हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की हर प्रकार की सेवा करने में मुझे असीम सुख अनुभव होता है। मैं शिक्षाप्रद विनोद से भरपूर हूँ, एक छोटा लड़का भी मेरे साथ निःसंकोच विनोद कर सकता है।
कृपया आप यहाँ आयें और आश्रम में कुछ समय रहें। आपके विचार बदल जायेंगे।
१४८
क्या यति धर्म से प्रबोधन प्राप्त हो सकता है?
यति धर्म वास्तव में भक्तिमय साधना अथवा आध्यात्मिक ध्यान के उद्देश्य से इन्द्रिय-संयम और मानसिक एकाग्रतापूर्ण जीने का तपस्वी जीवन है। सच्चे तपस्वी जीवन में निश्चित रूप से आचरण के और नैतिकता के कठोर नियमों का अनुपालन करना होता है जिसके आधार पर उच्च साधनाएँ की जाती हैं। तपपूर्ण जीवन प्रबोधन प्राप्ति का साधन है। इससे ध्यान का आधार तैयार हो जाता है और ध्यान ही फिर विवेक और साक्षात्कार प्राप्ति की ओर ले जाता है। कभी-कभी तपस्या का संकुचित अर्थ केवल शारीरिक कष्ट देने से ही ले लिया जाता है। किन्तु यह भारी भूल है तथा वासनाओं को शान्त किये बिना और मन को अनुशासित किये बिना केवल शारीरिक तप से प्रबोधन प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते।
१४९
जीवन और मृत्यु-इन दोनों में से अधिक भयानक क्या है?
जीवन और मृत्यु का क्रम, विकास की एक श्रृंखला है जो कि जीवात्मा के नये-से-नये अनुभवों के द्वारा, जीवात्मा की पूर्णता प्राप्ति की वास्तविक इच्छा की ओर उसे अग्रसर करती है। जीवन नाटक का एक दृश्य है जहाँ जीवात्मा कुछेक उन इच्छाओं को ले कर एक पोशाक अथवा रूप ले कर आती है जो कि उस प्राप्त विशेष समय और स्थान में पूरी की जा सकती है; और मृत्यु वह समय है जब जीवात्मा पर्दे के पीछे चली जाती है तथा नयी पोशाक पहन कर जीवन के दूसरे दृश्य में उन अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए तैयार हो कर आ जाती है जो वर्तमान देश-काल में पूर्ण किये जा सकने योग्य नहीं थीं तथा जिन्हें अन्य उपयुक्त समय और स्थान-विशेष की आवश्यकता होती है। अतः इसे यदि भलीभाँति समझ लिया जाता है तो दोनों में से कोई भी भयानक नहीं रहता। पूर्णता प्राप्ति की प्रक्रिया में बाधाओं को तोड़ने और आवरणों को भंग करने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। अज्ञानी मनुष्य के लिए तो दोनों ही अनुभव भयप्रद हैं। वह मृत्यु के अधिक भयानक होने की कल्पना करता है।
१५०
यह पृथ्वी क्या है?
विभिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी जा सकती हैं। शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के फल को भोगने के लिए तथा नये कर्म करने के लिए निर्धारित क्षेत्रों में से यह एक क्षेत्र है। यह भोग-भूमि और साथ ही कर्म-भूमि भी है। यह परमाणुओं का समूह है, ऊर्जा का रूप है, विचारों का भौतिकीकरण है, उन जीवात्माओं के कर्मों के प्रभावों की अभिव्यक्ति है, जिनसे यह बनी है और जिनसे यह सम्बन्धित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह पृथ्वी केवल उन ग्रहों में से एक ग्रह है जिनसे मिल कर यह समस्त विश्व बना है।
१५१
एक आश्रम में, जहाँ आपने युवा जिज्ञासु साधकों को इस विश्वास को दिलाते हुए एकत्रित किया है कि आप उन्हें जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्रता से बढ़ने में निर्देशित करेंगे, आप नृत्य, नाटक और संगीत को प्रोत्साहन क्यों देते हैं?
यह प्रश्न संगीत और नृत्य के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति अज्ञान को प्रकट करता है। संगीत और नृत्य दिव्य हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप स्मरण करें कि भगवान् श्री कृष्ण का अपनी अविच्छिन्न वंशी के साथ का स्वरूप तथा सरस्वती माता का वीणा सहित रूप सदैव हमें संगीत की दिव्यता की याद दिलाता है। भगवान् नटराज आपको स्मरण कराते हैं कि नृत्य का उद्गम उनसे होता है। मनुष्य की दुष्ट बुद्धि तो किसी का भी दुरुपयोग कर सकती है। यदि उत्सव-पर्व के समय मन्दिर में जेबकतरों की भरमार पायी जाती है, तो क्या हमें भगवान् के दर्शन से प्राप्त होने वाले आशीर्वादों को नकार देना चाहिए?
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संगीत और नृत्य कला को इन्द्रियजन्य मनोरंजन के स्तर तक गिरा दिया गया है। प्रत्येक प्रभु-प्रेमी एवं ललितकला-प्रेमी का यह पावन कर्तव्य है कि इन कलाओं को पवित्रता और दिव्यता के अपने वास्तविक उच्च स्तर तक ऊपर उठायें।
संगीत नादयोग है। यह तत्काल ही आपका नादब्रह्म, पावन प्रणव के साथ तादात्म्य स्थापित कर देता है। नृत्य आपको भाव-समाधि में प्रवेश पाने में सक्षम करता है।
नाटक आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार का अत्यन्त सशक्त साधन है। जो-कुछ आप सैकड़ों पुस्तकों से और घण्टों तक प्रवचन देने से नहीं सिखा पाते, वह अत्यन्त सरलता और प्रभावशाली ढंग से एक ही नाटक के द्वारा श्रोताओं को समझा सकते हैं। नाटक, कला का वह रूप है जो हृदय को सीधा स्पर्श करता है।
यही तथ्य कि सांसारिक मानव इन तीनों में इतनी अधिक रुचि लेता है और अपने दुष्टतापूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इनका दुरुपयोग करता रहा है, यह दर्शाता है कि कितनी गहन शक्ति इनमें मानव-हृदय एवं आत्मा को स्पर्श करने की है। यदि इनका आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सदुपयोग किया जाये तो वे धन्य हो जायेंगे।
१५२
स्वामी जी, आपने मानवता की सेवा के सक्रिय क्षेत्र में स्वयं को क्यों नहीं लगाया, जैसे कि गाँधी जी ने किया था, वैसे ? आपने उनकी तरह न करके, राजनैतिक क्षेत्र में किंचित् भी प्रवेश न करते हुए स्वयं को गंगा तट पर एकान्त जीवन व्यतीत करने के लिए क्यों चुन लिया ?
भगवान् ने प्रत्येक व्यक्ति को कतिपय गुणों से सम्पन्न करते हुए उनके लिए सेवा के अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किये होते हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि स्वयं में उन गुणों को खोज कर भगवान् की इच्छानुसार मानवता की निःस्वार्थ सेवा में उपयोग किया जाये। गाँधी जी की सेवा का राजनैतिक क्षेत्र है। मेरा सेवा-क्षेत्र त्याग, संन्यास और निवृत्ति-मार्ग का है। हमारा दोनों का सेवा-क्षेत्र का परिवर्तन तो ऐसे ही हो जायेगा जैसे मोची और दर्जी एक-दूसरे से कार्य परिवर्तित कर लें।
किन्तु आप अपने मन में इस विचार को घर न करने दें कि जो व्यक्ति राजनैतिक क्षेत्र में कार्यरत है केवल वही प्रभु की सन्तान की सेवा कर सकता है।
१५३
आत्महत्या करना पाप क्यों माना जाता है?
जीवन में सुख और दुःख क्रमशः मनुष्य के पुण्य और पापपूर्ण कर्मों का फल होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कष्ट झेल रहा है तो यह उसको यह याद दिलाने के लिए अनुस्मारक के रूप में आता है कि वह अपने जीवन को भला बनाये और भले कार्यों, आत्म-अनुशासन और सही प्रयासों के द्वारा भविष्य को सुखपूर्ण बना ले।
जब किसी व्यक्ति को अपराध करने के कारण न्यायालय द्वारा दण्डित करके कारागार में भेज दिया जाता है और वह व्यक्ति कारागार से निकल भागता है तो न्याय कहता है कि उसे पुनः कारागार में ही नहीं डाला जाये अपितु साथ ही और भी अधिक कठोर दण्ड दिया जाये, क्योंकि एक अपराध करने के अतिरिक्त उसने दण्ड से बच कर भागने का दूसरा अपराध भी किया है। यही नियम अपने कष्ट को झेलने से बचने के प्रयास में आत्महत्या करने पर लागू होता है, क्योंकि व्यक्ति को परमात्मा के विधान को स्वीकार करते हुए आत्म-सुधार करके भविष्य को सँवारने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा दार्शनिक विचारों को स्वीकार करते हुए कष्ट भोगने से बचने का अनुचित प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा न करने से भगवान् से भी और अधिक दण्ड मिलता है।
इसके अतिरिक्त, मनुष्य को जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं है। भले ही वह उसका अपना जीवन ही क्यों न हो। क्योंकि यह भगवान् की दृष्टि में ही पाप नहीं है, न्याय की दृष्टि से भी अपराध है। जो मनुष्य आत्महत्या कर लेता है वह सूक्ष्म-शरीर में, उतने ही समय तक और अधिक कष्ट पायेगा और फिर अपने कर्मों को भोगने के लिए निम्न योनि में जन्म लेगा। इस प्रकार आत्महत्या करना किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुँचाता।
१५४
'आत्मा शरीर से भिन्न है और शरीर द्वारा किये गये किसी भी कार्य का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर का अपने कर्मों के अनुसार अनेकों बार पुनर्जन्म होता है और परमात्मा की इच्छानुसार यह जन्म-मरण के चक्र में भटकता रहता है।' यदि ऐसा है, तो फिर स्वर्ग अथवा नरक में कौन जाता है ?
किसी भी प्रकार का वास्तविक भोक्ता, व्यक्तिगत रूप में, न तो आत्मा है न ही शरीर। यह मन है जो व्यक्तित्व का केन्द्र है, यह आत्मा के प्रकाश को ले कर उससे प्रकाशित हो कर अपना व्यक्तित्व बना लेता है जिसे जीवात्मा कहते हैं। और यह मन ही है जो सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग के सुख अथवा नरक के दुःख भोगता है, अथवा स्थूल या सूक्ष्म शरीर द्वारा किसी भी प्रकार के अनुभव करता है।
आत्मा का प्रकाश इस मन के ऊपर प्रतिबिम्बित होने के कारण ही यह मन चेतन प्रतीत होता है, जो कि वस्तुतः अपने आप में, अपनी रचना में ही सीमित है। अतः किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व उतना ही वास्तविक, अथवा सत्य है जितना कि किसी वास्तविक वस्तु-पदार्थ का प्रतिबिम्ब।
यद्यपि सब-कुछ परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है, तथापि मनुष्य के कर्म उसके होने वाले अच्छे या बुरे अनुभवों को, परमात्मा की इच्छानुसार निर्धारित करते हैं। यह सभी अनुभव न तो आत्मा को होते हैं न ही शरीर को । यद्यपि इनका साधन स्थूल शरीर बनता है, किन्तु अनुभव मन ही करता है।
१५५
हम प्रायः अत्यन्त भले व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट झेलते हुए पाते हैं। ऐसा क्यों है? उत्तर में कह सकते हैं, "उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण।" यह क्या हम सृष्टि-रचना के आरम्भ तक के पिछले कर्मों को इसका कारण कह सकते हैं।
कर्म का सिद्धान्त अटल है। प्रत्येक मनुष्य अपने विगत जन्मों के फल भोगता है। भला व्यक्ति अधिक कष्ट भोगेगा, क्योंकि वह आध्यात्मिक पथ पर बहुत शीघ्र आगे बढ़ना चाहता है। उसने बहुत से बुरे कर्मों का भुगतान, इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से, कर लेना होता है। किन्तु भगवान् अपनी कृपा से उसे अद्भुत सहनशक्ति प्रदान कर देते हैं। भले व्यक्ति अथवा जिज्ञासु साधक को अनेक कठिनाइयाँ और कष्ट सहन करने पड़ते हैं। किन्तु भगवान् की कृपा से वह इन सबमें भी अत्यन्त प्रसन्न रहता है। वह स्वेच्छा से इन कष्टों का स्वागत करता है। इस संसार में केवल दुःख-दर्द और कष्ट ही सर्वोत्तम हैं, क्योंकि यह भगवान् की ओर का पथ दशति हैं।
१५६
भक्ति में वृद्धि कैसे की जा सकती है?
सत्संग के द्वारा, भगवन्नाम-स्मरण, कीर्तन, कथा-श्रवण करके, रामायण, भागवत का अध्ययन करके, भक्तों के जीवनचरित-भक्त विजयम् और भक्त लीलामृत का स्वाध्याय-विष्णुसहस्रनाम, नारद भक्ति सूत्र और शाण्डिल्य सूत्रों का पाठ करके भक्ति-भाव को बढ़ाया जा सकता है। आपको निश्चित रूप से स्वयं में वैराग्य विकसित करना होगा। यह अत्यन्त आवश्यक है। भक्तों के सान्निध्य में रहें। अयोध्या में निवास करें। आपमें भगवान् श्री राम के प्रति भक्ति बढ़ेगी। वृन्दावन में वास करें। भागवत पढ़ें। द्वादशाक्षर मन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें। आपमें कृष्ण-भक्ति का विकास होगा।
१५७
यह संसार ईश्वर की एषणा मात्र का परिणाम है। उस एषणा से कम अथवा उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर तो हर समय हर एक बात के लिए आदेश नहीं देता रहता ! ऐसा होने से तो वह अत्यधिक व्यस्त हो जायेगा। इसका अर्थ तो यह है कि सब-कुछ पूर्व-नियोजित है, अतः व्यक्ति के पुरुषार्थ का कोई स्थान नहीं है।
यह धारणा कि ईश्वर कुछ बातों में ही आदेश देता है-हर समय, हर बात में नहीं, क्योंकि ऐसा करने से तो वह बहुत ही अधिक व्यस्त हो जायेगा, निर्मूल है। ईश्वर अपनी दिव्य शक्ति से एक ही क्षण में सब-कुछ देख सकता है। उसके 'अत्यधिक व्यस्त' हो जाने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे काम करने के लिए मनुष्य की भाँति इन्द्रियों का उपयोग नहीं करना पड़ता। ईश्वर मनुष्य की तरह अलग-अलग सोचते हुए कार्य नहीं करता; क्योंकि ईश्वर के कार्य उस अविच्छिन्न, सदैव-जागरूक, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा-जो न कभी निद्राग्रस्त होता है, न ही आराम करता है-से भिन्न नहीं है। ईश्वर वस्तुतः सर्वसमर्थ परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही है। समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड की रचना उस परमात्मा की सृष्टि-रचना की इच्छा मात्र से ही निर्धारित है। किन्तु इस निर्धारण का अर्थ मनुष्य के पुरुषार्थ को नकारने से नहीं है। मनुष्य में स्वयं अपने विषय में और अपने से सम्बन्धित बाह्य जगत् के विषय में अपेक्षाकृत अधिक समझ है तथा वह विवेक-शक्ति और कार्य करने की शक्ति से भी सम्पन्न है। यद्यपि विश्व के और मनुष्य के व्यक्तिगत सभी कार्यों का आधार ईश्वर है तथापि ईश्वर व्यक्ति के निजी कार्यों में लिप्म नहीं है। ईश्वर के कार्यों में सब-कुछ पूर्व-नियोजित है। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब-कुछ केवल ईश्वर में, और ईश्वर पर ही घटता है। किन्तु व्यक्ति के निजी सीमित दृष्टिकोण के अनुसार, अपरिवर्तनीय वैश्व-नियम के तथ्य के होते हुए भी, उसके अपने व्यक्तिगत कार्यों में एक स्वतन्त्रता, उसके अपने व्यक्तित्व के कारण ही उसने आरोपित कर ली है। यद्यपि व्यक्ति के सोचने और कर्म करने की स्वतन्त्रता, इस सम्बन्ध में अन्तिम सत्य नहीं है, फिर भी यह अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है और व्यक्ति को उसके कार्यों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित करना आरम्भ कर देती है, क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं को कर्ता मान लिया होता है। इस स्व-निर्मित बन्धन के परिणामस्वरूप जीव कष्ट भोगता है तथा जैसे ही जीव अपनी आत्मा का ईश्वर के साथ ऐक्य को अनुभव कर लेता है, उसी क्षण से उसके कष्टों का अन्त हो जाता है।
१५८
क्या एक पूर्ण विकसित योगी को अपनी योग-शक्तियों की परीक्षा करने की इच्छा नहीं होती? क्या यह परीक्षण करना उचित है?
पूर्ण रूप से विकसित योगी को कभी भी स्वयं का अथवा अपनी शक्तियों का परीक्षण करके देखने का विचार नहीं आ सकता। यदि ऐसा हो तो उस व्यक्ति को पूर्ण विकसित योगी नहीं समझना चाहिए। केवल कच्चे, अधपके या अधूरे साधक अथवा योगी ही अपनी या फिर अपनी अर्जित शक्तियों की परीक्षा करने के इच्छुक हो सकते हैं, और इन शक्तियों से उपलब्ध हुई अपनी उन्नति को जाँचना चाह सकते हैं।
योग शास्त्रों में निर्धारित नियमों के अनुसार योगी में योग-शक्तियों का प्रकटन उसकी योग में प्राप्त की गयी उन्नति के अनुपात में ही होता है और यदि वह स्वयं की परीक्षा के लिए अथवा योग्यता-प्रदर्शन के लिए जरा-सा भी प्रयत्न करता है तो उसकी और आगे उन्नति करने में निश्चित रूप से हानि होती है। योग साधक के किंचित् भी इच्छा न करने पर भी प्रति दिन, प्रति मिनट, नहीं; अपितु प्रत्येक क्षण ही कोई-न-कोई आनन्दपूर्ण अनुभूति उसे होती ही रहती है, क्योंकि ऐसे अनुभव स्वयं अपने-आप ही आते हैं। अतः साधक को भगवान् की अद्भुत महिमा को समझते हुए इन अनुभवों के प्रति तटस्थ ही रहना चाहिए और इन अनुभवों के विषय में जानने-सोचने की चिन्ता भी नहीं करनी चाहिए अर्थात् इनसे सम्बन्ध जोड़ने अथवा आनन्द-रस लेने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। तभी और केवल तब ही वह इस पथ पर और अधिक उन्नति कर सकता है। पूर्ण विकसित योगी वह होता है जिसने योग के मार्ग को अपना कर आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, अतः उसमें कभी भी यह जानने के लिए कि वह कौन है और उसने इन प्राप्त शक्तियों के द्वारा कितनी उन्नति की है, किंचित् भी जिज्ञासा नहीं होती।
१५९
कोई व्यक्ति जब संन्यास लेने के लिए अचानक समस्त सांसारिक सम्बन्धों को तोड़ देता है, तब उसे कैसा लगता है?
किसी भी व्यक्ति में जब त्याग की तीव्र भावना होती है तो संसार का अथवा पुराने सम्बन्धों का कुछ भी विचार उसके मन में नहीं रहता। यदि अनिवार्य वैराग्य के न होने पर भी वह संन्यास ले लेता है तब भी आवश्यक नहीं है कि उसे पुराने सम्बन्ध छूटने का कोई भाव मन में हो, यद्यपि सुप्त वासनाएँ, वृत्तियाँ या संस्कार उसके मन में पड़े रह सकते हैं। सच्चा संन्यासी जब समस्त सांसारिक सम्बन्धों का त्याग करता है तो उसे अत्यन्त आनन्द मिलता है।
१६०
मैंने 'माई मैगज़ीन' में आपके लेख पढ़े हैं-"नारी केवल मल-मूत्र, मवाद, मांस-रक्त से भरा हुआ दुर्गन्धपूर्ण मांस का थैला मात्र है।" नारी-जाति का हम इस प्रकार कैसे दुत्कारते हुए विरोध कर सकते हैं? मेरा तो विचार है कि इस संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं है।
आवश्यकता से अधिक पढ़ना और जीवन में कुछ भी न उतारना, भ्रमित कर देता है। कामी पुरुषों में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैं स्त्रियों के विषय में ऐसा नकारात्मक चि प्रस्तुत करता हूँ। वास्तव में नारियाँ शक्ति का प्रकटित रूप हैं। हाँ, सब-कुछ पावन है। सब-कुछ पवित्र है। सब सुन्दर है। केवल आध्यात्मिक पथ पर उन्नत व्यक्ति इसे अनुमद कर सकते हैं। नये-नये प्रारम्भिक लोग इस मन्त्र को केवल तोते की तरह रट सकते हैं। उनके अनुभव, दृष्टि और साधना के ढंग अनुभूति-प्राप्त साधकों की अभिव्यक्ति से भिन्न होते हैं। प्रारम्भिक साधकों को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा सरलता से धोखा खा जायेंगे।
१६१
आजकल राजनीति भगवान् बन गयी है, और विशेष रूप से भारत में तो ऐसा ही है। धर्म को एक अनावश्यक वस्तु माना जाने लगा है। तब फिर ऐसी स्थिति में क्या हर व्यक्ति को भगवान् में और धर्म में विश्वास करा पाना सम्भव है?
राजनीति को धर्म से ऊपर माना जाता है, ऐसा समझना गलत है। अपने व्यक्तिगत जीवन में अधिकांश लोग भगवान् में विश्वास रखते हैं। और भारत में तो सारी धरा के अन्तर्निहित धर्म की लहर विचरती है। राजनीति केवल सतही गतिविधि मात्र है ज अधिकांश लोगों पर सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों द्वारा लाद दी गयी है।
जब व्यक्ति को चारों ओर से विपत्तियाँ घेर लेती हैं, जब इन्द्रिय-विषय-वस्तुओं की नश्वरता के कारण वह निराश हो जाता है, जब तरह-तरह के सुख-दुःख के अनुभव मिलने से उसका विवेक और वैराग्य उदय होता है तब उसका मन भगवान् की ओर उन्मुख होता है। अब धर्म के प्रभाव के प्रति वह ग्रहणशील हो जाता है और भले लोगों का सग तथा आध्यात्मिक पुस्तकों का साथ उसे धार्मिक बना देता है। ऐसी अवस्था तक पहुंचने से पहले मनुष्य पर बलपूर्वक धर्म थोपने का कोई लाभ नहीं है।
१६२
क्या आत्मा एक वर्ष में पुनः नया शरीर धारण कर लेती है ? अथवा ऐसा होने में दश वर्ष लग जाते हैं? पुनः इस धरती पर आने से पहले जीवात्मा कितने समय तक सूक्ष्म लोकों में रहती है ?
इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। मुख्य रूप से दो तत्त्व इसको निर्धारित करने वाले हैं। व्यक्ति के निजी कर्म तथा मृत्यु के समय की अन्तिम स्थिति। यह समय का अन्तराल सैकड़ों वर्षों से ले कर कुछ मास मात्र तक के बीच का भी हो सकता है। जिन्हें अपने कुछ कर्मों का फल अन्य सूक्ष्मतम लोकों में भोगना होता है, उन्हें नया शरीर मिलने से पहले पर्याप्त समय लग जाता है। यह अन्तराल बहुत दीर्घ अवधि का होता है, क्योंकि पृथ्वी का एक वर्ष देवलोक के एक दिन के बराबर होता है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण मिलता है कि अति प्राचीन स्मारकों के ध्वंसावशेषों को देख कर आश्चर्य और प्रशंसा करते हुए विदेशी यात्रियों को देख कर एक सन्त, जो वहाँ एकान्त में बैठे हुए थे, ने कहा कि शताब्दियों पूर्व इन्हीं में से कुछ लोगों ने इन स्मारकों का निर्माण किया था।
अति विषयी व्यक्ति, जिसकी कोई अति तीव्र लालसा अथवा गहन आसक्ति शेष रह जाती है, वह कई बार तुरन्त पुनर्जन्म प्राप्त कर लेता है। कई बार अचानक अपमृत्यु से अथवा अचानक दुर्घटना से मृत्यु हो जाने से जीव बहुत शीघ्र पुनः जन्म ले लेता है। प्रायः ऐसी घटनाओं में अति शीघ्र नये शरीर में आने पर जीव को गत जन्म की कई घटनाओं की स्मृति बनी रहती है। वह अपने पिछले जन्म के सम्बन्धियों, मित्रों और अपने पुराने आवास-स्थल तक को, वहाँ की वस्तुओं तक को पहचान लेता है। कभी-कभी तो ऐसी घटनाओं से विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जहाँ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी गयी थी, पुनः जन्म लेने पर अपनी हत्या के किये जाने का ढंग और हत्यारे की रूपरेखा तक वर्णन कर देता है, यह घटना बहुत अधिक पुरानी नहीं है।
किन्तु तत्काल पुनर्जन्म की ऐसी घटनाएँ अधिक नहीं हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए प्रायः मृत्यु और पुनः शरीर धारण करने में इस पृथ्वी के समय के अनुसार काफी लम्बा समय व्यतीत हो जाता है। अधिक भले काम करने वाले भले लोग दिव्य लोकों में दीर्घ काल व्यतीत करने के उपरान्त पुनः धरती पर आते हैं। महान् आत्माएँ, उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचे हुए लोग पुनः धरा पर आने से पहले दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करते हैं।
१६३
संगीत क्या है? दुःखी मन को शान्त करने की कोई शक्ति क्या संगीत में है?
संगीत एक सुरीली, मधुर और लय-ताल-बद्ध ऐसी प्रणाली है जो आन्तरिक शान्ति और अवर्णनीय आनन्द प्रदान करने की क्षमता रखती है। संगीत विज्ञानों में से एक ऐसा विज्ञान है जो उस नाद (शब्द) से सम्बन्धित है जो परब्रह्म द्वारा प्रकटित प्रणव- का आदि स्वर है। सभी सातों स्वर-सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी-जिनसे बाद में विविध शब्द युक्त उच्चारण बने, सर्वप्रथम इस मूल ॐ जो ब्रह्म का प्रतीक है, से ही निकले हैं। संगीत ललितकलाओं में से एक कला है। हाँ, इसमें केवल विषादग्रस्त मन का शान्ति प्रदान करने की ही शक्ति नहीं है, अपितु स्नायविक दुर्बलता, अनिद्रा, मिर्गी, अवमार और चक्कर आना इत्यादि अनेक रोगों की चिकित्सा करने की क्षमता भी इसमें है। सगीत शास्त्र में पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्म के साथ समस्वरता स्थापित करना आवश्यक है। ब्रह्म परिपूर्ण प्रकाश, परम ज्ञान, परम आनन्द स्वरूप है इसी प्रकार वह परम नाद स्वर हैं। परमात्मा नाद ब्रह्म हैं। व्यक्ति संगीत के माध्यम से भगवान् को पा सकता है, जैसे त्यागराज, पुरन्दरदास, तुकाराम तथा अन्य कई भक्तों ने प्राप्त किया था।
१६४
यदि सब-कुछ भगवान् के ही निर्देशानुसार होता है तो जब तक वे मेरे द्वारा दोषी को दण्ड न दिलवाना चाहते हों तब तक यह सम्भव नहीं है कि मैं किसी की हत्या करूँ या चोरी करूँ। भोक्ता के कर्म फलित होने हैं, अतः उसकी मृत्यु अथवा अन्य कुछ भी हानि होना निश्चित है। यदि उसे मृत्युदण्ड नहीं दिया गया तो इस सृष्टि का सारा ढाँचा चरमरा जायेगा। इसीलिए भगवान् की इच्छापूर्ति के उद्देश्य से ही उस भोक्ता के सम्पर्क में मुझे लाया गया। फाँसी देने वाले को शासन अपना कार्य करने के लिए वेतन देता है। इसी प्रकार पाप कर्म के फलस्वरूप दण्ड मिलने की जगह मुझे भी भगवद्-इच्छा पूर्ण कर देने के फलस्वरूप पुण्य फल अथवा पारितोषिक क्यों नहीं मिलना चाहिए? हिटलर भगवान् की इच्छा के बिना युद्ध करके इतना नर-संहार नहीं कर सकता था। उसे दोष देना तो व्यर्थ है न ?
भगवान् ही सर्वनियन्ता है और वही सब-कुछ करने वाले हैं; किन्तु तो भी जब मनुष्य यह समझता है कि वह कर्ता है, तब वह उस कार्य का अच्छा अथवा बुरा जो परिणाम हो, उसका भोक्ता भी निश्चित रूप से बनता है। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि अनुचित कर्म केवल तभी सम्भव होता है जब व्यक्ति जीवभाव में अथवा अहंभाव में हो, न कि तब सम्भव हो सकता है जब व्यक्ति परमात्म-साक्षात्कार प्राप्त हो, ईश-प्रेरित हो अथवा भगवान् का उपकरण मात्र हो।
जीव यह नहीं सोच सकता कि दोषी की हत्या करने की उससे अपेक्षा की जाती है और यह उसे ईश्वरेच्छा से उपलब्ध करायी गयी है, क्योंकि जीव सर्वज्ञ नहीं है, जब तक बह परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होने की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह यह नहीं जान सकता कि वस्तुतः भगवान् की इच्छा क्या है। किसी भी जीव को इस गलत धारणा में नहीं फँसना चाहिए कि दोषी व्यक्ति की हत्या करके उसके कर्मों का फल देने का अधिकार उस व्यक्ति को भगवान् ने दिया है। इस मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाले को अपने किये का फल अत्यन्त भीषण एवं असहनीय कष्टों के रूप में भोगना ही पड़ेगा।
भगवान् किसी भी जीव से सीधा नहीं कहते कि उसे किसी की हत्या करनी अथवा कहीं चोरी करनी है और यदि जीव ऐसा अनुचित कार्य करने की गलती करता है तो केवल वही उत्तरदायी है, भगवान् नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान् किसी व्यक्ति को निर्देश दें कि अमुक दुष्कर्म करो अथवा किसी की हत्या करो, किसी को हानि पहुँचाओ अथवा कोई भी ऐसा कार्य जिसमें किसी अन्य को कष्ट पहुँचता हो, वह करो। ऐसे सभी अनुचित कुकर्म व्यक्ति के अज्ञान और भ्रान्ति के परिणाम होते हैं तथा उन्हें करने वाले को दण्ड भोगना पड़ता ही है। दिव्य गतिविधि तो सदैव स्वतन्त्रता की ओर, परिपूर्णता, शान्ति और आनन्द की ओर अग्रसर करती है तथा वह किसी भी प्रकार से किंचित् भी दुःख-दर्द का कारण नहीं है।
१६५
यदि मैं ऋषिकेश आ जाऊँ तो क्या मुझे मानसिक शान्ति प्राप्त हो सकती है, क्या मुझे आध्यात्मिक स्पन्दनों की अनुभूति हो सकती है?
हाँ, ऐसा हो सकता है। किन्तु जब आपने यहाँ आना हो, तो अकेले आयें। यदि मित्र-मण्डली को साथ लायेंगे तो उनके साथ सब तरह के वार्तालाप से वही सांसारिक वातावरण रच लेंगे। आयें और महात्माओं के दर्शन करें। उनके आध्यात्मिक निर्देशनों का श्रवण करें। उनके साथ रहें। मौन रहें और एकाग्रता एवं ध्यान का अभ्यास करें। केवल तभी आप शान्ति का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे।
१६६
मैं सेवा-निवृत्त हो चुका हूँ। मैंने अपने बेटों को अच्छी नौकरियों में लगा दिया है। अब मुझे योगी का जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करना चाहिए?
मोह को नष्ट करना अत्यन्त कठिन है। यह माया का अत्यन्त सशक्त अस्त्र है। यह मोह ही 'मैं, मेरा' की और 'अहंकार' की भावना उत्पन्न करता है। यह सन्तान के प्रति अन्ध-प्रेम उत्पन्न करता है। आप अपने हृदय से अभी मोह को नष्ट नहीं कर सके हैं। अपनी पत्नी से, बच्चों से, मित्रों और सभी सम्बन्धियों से समस्त सम्बन्ध काट डालें। पत्र भी न लिखें। तीर्थयात्रा पर जायें और वहाँ महात्माओं के दर्शन करें। वैराग्य विकसित करें। अपने निजी अनुभव से आपने देख लिया है कि सांसारिक जीवन से आपको परम शान्ति और आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आपमें सचमुच ही मोह नहीं है और यदि आपके मन में संन्यासी बनने की तीव्र इच्छा है तो संन्यासी हो जायें। महिमाशाली तपस्वी जीवन जियें और योग-साधना द्वारा आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करें। अपनी यात्रा के अनुभव के आधार पर ऐसे गुरु का चयन कर लें जो आपको निर्देश दे और फिर उन निर्देशों का पूर्णतया पालन करें।
१६७
क्या पत्नी और बच्चों के होते हुए मैं संन्यास ग्रहण कर सकता हूँ? क्या असहाय अवस्था में अपने आश्रितों को छोड़ कर चले जाना पाप नहीं है?
यदि आपमें विवेक से उत्पन्न सच्चा वैराग्य है और यदि आपमें गहन तितिक्षा एवं तीव्र मुमुक्षुत्व है, तो आप संन्यास ले सकते हैं। श्रुतियों का कथन है कि जिस क्षण आपमें वैराग्य आ जाये, उसी क्षण संसार को त्याग दें। यदि आपके मन में अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति मोह है तो आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन सदैव उनके सम्बन्ध में ही सोचता रहेगा। अतः पहले मोह को नष्ट करें। सच्चा वैराग्य विकसित करें।
संसार में जब तक हैं, यथासम्भव जप और ध्यान करें। जब इसमें कुछ उन्नत हो जायें तो सुदूर क्षेत्र में चले जायें, एकान्त में रहें, अपने मन की सामर्थ्य को जाँचें और देखें कि क्या अभी आपके मन में मोह कहीं अटका हुआ तो नहीं है! तब आप संन्यास ले सकते हैं। आप सफल होंगे।
संन्यास से पहले देख लें कि आपकी पत्नी और बच्चे भलीभाँति आत्मनिर्भर हैं? अन्यथा वे सतत आपके सम्बन्ध में सोचते रहेंगे और उनका चिन्तन आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। पत्नी के साथ रहते समय उसे संन्यास का महत्त्व समझाएँ और उसे जप और ध्यान करने के लिए कहें। उसे भी अवश्यमेव आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। केवल तभी वह आपके संन्यास ले लेने के बाद आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
भर्तृहरि, गौरांग, सदाशिव ब्रह्मेन्द्र और अन्यों ने अपनी पत्नियों को त्याग दिया था। संन्यास के उपरान्त उन्होंने कभी अपनी पत्नियों का चिन्तन नहीं किया। क्या उन्हें आत्म-साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ? क्या उन्हें कोई पाप अथवा शाप ने स्पर्श किया? आपने यदि अपने परिवार का भलीभाँति प्रबन्ध नहीं भी किया तो भी यदि आपमें वास्तविक वैराग्य है तो आप संन्यास ले सकते हैं। बस अपने परिवार से स्वयं को अलग कर लें और फिर देखें कि उनकी ठीक प्रकार से देख-रेख हो रही है या नहीं। रामतीर्थ ने छोटे-छोटे दो बच्चों सहित अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, बिना उनका कुछ प्रबन्ध किये। किन्तु उनका बड़ा पुत्र इंजीनियर बना और छोटा प्रोफेसर । भगवान् में पूर्ण विश्वास रखें।
१६८
मेरा मन चंचल है और शरीर निर्बल है। एकाग्रता के प्रयासों में कभी सफलता भी मिल जाती है, किन्तु अधिकतर अन्त में निराशा का ही सामना करना पड़ता है। कृपया मेरी सहायता कीजिए।
सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। सही आहार एवं आसन-प्राणायाम के हल्के-फुल्के व्यायाम द्वारा सुस्वस्थ बनें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। फिर धीरे-धीरे इच्छाओं, चिन्ताओं, तनावों, कल्पना-लोक के निर्माण के स्वभाव तथा दुर्गुणों को नष्ट कर दें। सन्तुष्ट जीवन जियें। लोक-व्यवहार को कम कर दें। हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी इत्यादि जैसे आध्यात्मिक वातावरण वाले स्थान में निवास करें। पूरे तीन मास तक मौन-व्रत का पालन करें। आप अत्यन्त सरलता से मन को नियन्त्रित कर लेंगे।
१६९
मैं अपनी आँखों में जलन और मन में चंचलता का अनुभव करता है, अतः ध्यान करने में अक्षम हूँ। क्या इसके लिए कोई प्रभावशाली उपाय है?"
इससे यह प्रकट होता है कि आपकी प्रकृति में उष्णता है। प्रातः अपने शिर में आँवला तेल अथवा मक्खन लगायें और उसके उपरान्त स्नान करें। सात्त्विक आहार लें। जब भी प्यास लगे, मिश्री-शर्बत का पान करें। प्रातःकाल और रात को सोने से पहले एक प्याला शुद्ध गाय का दूध पीयें। भोजन संयमपूर्वक और सही समय पर करें। दिन में दो बार स्नान करें। यह सब करने से आपकी प्रकृति में शीतलता आ जायेगी।
१७०
जब भी मैं त्रिकुटी पर ध्यान करने का प्रयत्न करता हूँ, तभी शिर में दर्द सा होने लगता है। क्या इसका कोई उपचार है ?
यदि त्रिकुटी पर ध्यान करने से शिर-दर्द होता है तो नासिकाग्र दृष्टि, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि केन्द्रित करें। इससे आपको लाभ होगा। मन के साथ संघर्ष न करें। आधा घण्टा आराम कर लें। यदि अभी भी दर्द हो रहा हो तो अपनी आँखें बन्द कर लें, फिर ध्यान करें।
१७१
क्या मेरे जैसा ४५ वर्ष की आयु का व्यक्ति हठयोग का अभ्यास आरम्भ कर सकता है? इस आयु में मुझे पूर्ण स्वास्थ्य और शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है?
हाँ, आपमें एकनिष्ठता, गम्भीरता, विश्वास, उत्साह और शक्ति निश्चित रूप से होनी चाहिए। ध्यानपूर्वक धीरे-धीरे और एक-एक पग आगे बढ़ना आवश्यक है। बहुत अधिक थक जाने से बचना चाहिए। यदि आप साथ-साथ मौन, मिताहार का पालन तथा जप और ध्यान का अभ्यास करेंगे तो योगाभ्यास से आपको सफलता प्राप्त होगी। आसन, प्राणायाम इत्यादि व्यक्ति के मूल स्वभाव और शारीरिक गठन पर निर्भर करते हैं। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अभ्यास होते हैं।
यदि आप बल और ओजस्विता प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी, इस क्षण से सच्चे ब्रह्मचारी बन जायें। मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करें। सात्विक आहार लें। वैराग्य को विकसित करें। मेरी पुस्तक, 'प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य' पढ़ें। उसमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए आपको व्यावहारिक अभ्यास मिल जायेंगे।
१७२
कैसे पता चल सकता है कि मेरी चित्त-शुद्धि हो गयी है या नहीं ?
यदि आपका चित्त शुद्ध हो चुका है तो आपके मन में कामुक विचार, सांसारिक इच्छाएँ, अपवित्र विचार, कामुक वासनाएँ, क्रोध, दम्भ, घमण्ड, अहंकार, लोभ अथवा ईर्ष्या इत्यादि के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। भोगविलासपूर्ण वस्तु-पदार्थों के प्रति आप आकर्षित नहीं होंगे। आपमें सुदृढ़ एवं स्थायी वैराग्य होगा। स्वप्न में भी कुविचार आपके मन में नहीं आयेंगे। आपमें दया, वैश्व-प्रेम, क्षमा, मन का समत्व और सन्तुलन जैसे दैवी गुण विकसित होंगे। ये चिह्न हैं जो संकेत देते हैं कि आपने चित्त-शुद्धि प्राप्त कर ली है।
१७३
हिन्दू लोग लिंग अथवा पुरुष की जननेन्द्री की पूजा करते हैं। वे अज्ञानी लोग हैं। उनके धर्म के कोई भी दार्शनिक सिद्धान्त नहीं हैं।
यह एक बुद्धिहीन, बेसमझ, उत्सुकतापूर्ण, कामुक और अशुद्ध-हृदयी विदेशी व्यक्ति का व्यंगपूर्ण कथन है। जब कोई विदेशी तमिल अथवा अन्य कोई हिन्दुस्तानी भाषा सीखने लगता है तो आरम्भ में ही उस भाषा के कुछेक भद्दे एवं असभ्य शब्द सीख लेता है। यह उसके स्वभाव की उत्सुकता के कारण होता है। इसी तरह अनोखे स्वभाव वाला विदेशी पूजा के प्रतीकों में दोष खोजने का प्रयत्न करता रहता है। लिंग वास्तव में भगवान् शिव के निराकार स्वरूप का केवल बाह्य प्रतीक है।
संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ चिह्न अथवा वाचक है। यह एक प्रतीक है जो अनुमान द्वारा निश्चय तक पहुँचने का संकेत करता है। जब आप नदी में आयी हुई बाढ़ को देखते हैं तो अनुमान द्वारा समझ लेते हैं कि निश्चित रूप से कल कहीं-न-कहीं भारी वर्षा हुई होगी। जब कहीं से धुआँ उठता देखते हैं तो अनुमान से जान जाते हैं कि वहाँ अवश्य ही आग जल रही होगी। असंख्य नाम-रूपों वाला यह विशाल जगत् उस सर्वशक्तिमान् परमात्मा का लिंग अथवा प्रतीक है। शिवलिग भगवान् शिव का चिहर अथवा प्रतीक है। जब आप शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उसी क्षण आपका मर ऊर्ध्वगमन करता है (उन्नत हो जाता है) और आप भगवान् शिव के सम्बन्ध में चिन्तर करने लगते हैं।
मन में एकाग्रता लाने की शिवलिंग में अद्भुत रहस्यमयी शक्ति है। जैसे हमारा पर स्फटिक को एकटक देखने से अत्यन्त सरलतापूर्वक केन्द्रित हो जाता है, बिलकुल तरह लिंग को निहारते ही यह एकाग्र हो जाता है। इसीलिए भारत के प्राचीन ऋषियों भगवान् शिव के मन्दिरों में लिंग स्थापना का विधान बताया है।
सच्चे भक्त के लिए शिवलिंग पत्थर का टुकड़ा नहीं है। यह उज्ज्वल तेजस अथवा चैतन्य है। यह लिंग उस भक्त से बात करता है और उसमें अश्रु प्रवाहित करने, रोमांचित करने और हृदय द्रवित कर देने की क्षमता है। यह भक्त को देह-बोध से उन्नत करके भगवान् से वार्तालाप करने तथा निर्विकल्प समाधि में ले जाने में सहायक बनता है। भगवान् राम ने रामेश्वर में शिवलिंग की पूजा की। रावण, जो कि ज्ञान-सम्पन्न पण्डित था, ने स्वर्णलिंग की पूजा की। लिंग में कितनी विलक्षण रहस्यमयी शक्ति होगी।
वस्तुतः सदाशिव से प्रकटित चैतन्य का प्रकाश ही शिवलिंग है। उनमें से हो जड़-चेतन मयी सम्पूर्ण सृष्टि की रचना होती है। वे प्रत्येक वस्तु के लिंग अथवा कारण हैं और अन्ततः समस्त जगत् उनमें ही लय हो जाता है। शिवमहापुराण का कथन है, "पीठ अम्बमयं सर्वं शिवलिंगश्च चिन्मयम्।" सबका आधार अथवा पीठ प्रकृति अथवा पार्वती है, और लिंग चिन्मय पुरुष, देदीप्यमान प्रकाश, स्वयं प्रकाशित प्रकाश है। प्रकृति और पुरुष का, पार्वती और शिव का मिलन संसार की उत्पत्ति का कारण है।
लिंग और योनि का संयोग, परब्रह्म परमात्मा के प्रकृति और चैतन्य पहलुओं के परस्पर मिलन का प्रकटीकरण है। यह उस पितृत्व और मातृत्व के आध्यात्मिक संयोग के सिद्धान्त का परिचायक है जिससे यह लौकिक नानात्व उत्पन्न हुआ है। यह परिवर्तनहीन परमात्मा और पराशक्ति का वह शाश्वत मिलन है जिससे समस्त परिवर्तनशील जगत् प्रकट होता है।
इस उदात्त विचार के चिन्तन-मनन से साधक की निम्न वासनापूर्ण प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। लिंग और योनि के अध्यात्मीकरण और दिव्यीकरण से साधक को कामुक विचारों से मुक्त होने में सहायता मिलती है। इस उदात्त विचारधारा से धीरे-धीरे समस्त तुच्छ विचार समाप्त हो जाते हैं। भगवान् शिव के अपनी माया शक्ति द्वारा, माया शक्ति में ही आत्म-सुख एवं आत्म-नानात्व के मूलभूत सृष्टि-रचना के सिद्धान्त में संसार के सभी कामुक सम्बन्धों का इस प्रकार अध्यात्मीकरण हो जाता है।
१७४
एकाग्रता अथवा धारणा के लिए सबसे सबल साधन क्या है?
भगवन्नाम का जप। और इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण और आवश्यक बात यह समझने की है कि पूर्ण एकाग्रता केवल एक-दो दिन में प्राप्त नहीं हो जाती; आपको कभी भी निराश हो कर प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। शान्त रहें। धैर्य रखें। यदि मन इधर-उधर भटकता है तो चिन्ता न करें। जप नियमपूर्वक करते रहें; ध्यान में बैठने के समय का पालन दृढ़ता से करें। धीरे-धीरे मन अपने-आप ईश्वरोन्मुखी हो जायेगा और एक बार इसे भगवान् के आनन्द का स्वाद मिल गया, 1, फिर कुछ भी इसे हिला नहीं पायेगा।
१७५
हमें अपने पिछले जन्मों का स्मरण क्यों नहीं रहता ?
हमारी सीमितताओं के होते हुए ऐसी स्मृतियों से हमारा वर्तमान जीवन दुरूह हो जाता। इसीलिए सर्वज्ञ एवं सुखदाता भगवान् ने हमारा मानसिक विकास इस तरह से निश्चित किया है कि हमारा पूर्व-जन्म तभी तक हमें स्मरण रहे जब तक वह स्मृति हमारे लिए अच्छी और सहायप्रद है। जन्म-मरण के चक्र के अन्तिम छोर पर पूर्ण विकसित अवस्था में पहुँच जाने पर, जीवन्मुक्त व्यक्ति को समस्त पूर्व-जन्मों की श्रृंखला का बोध हो जाता है।
१७६
पुनर्जन्म के विषय में उसके विरोध में यह कहा जाता है कि पिछले युगों की तुलना में अब जनसंख्या बहुत अधिक है।
यह आवश्यक नहीं है कि वही लोग पुनः इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, अन्य कोई नहीं। मानव-जीवन के क्रम-विकास में, अन्य बहुत से प्राणी भी निम्न योनि से विकसित हो कर मानव स्तर पर आते हैं। यह सब तो मानवेतर शक्तियों अथवा दिव्य शक्तियों द्वारा, भगवान् अथवा ईश्वर द्वारा स्वयं संचालित है। और फिर, यह भी आवश्यक नहीं है कि पुनर्जन्म इस पृथ्वी पर ही हो। यह पूरे विश्व ब्रह्माण्ड में अन्यत्र कहीं भी हो सकता है।
१७७
मैं एकादशी को उपवास करता हूँ। मैंने सुना है कि उपवास करने मनुष्य का जीवन-काल छोटा हो जाता है। क्या यह सत्य है?
बिलकुल नहीं। उपवास से शरीर, मन, प्राण और नाड़ियाँ सभी का नवीकरण जायेगा और अधिक सशक्त होंगे। समस्त अशुद्धताएँ और मल नष्ट हो जायेंगे। व्यि सात्त्विक गुणों का विकास बहुत सरलता से कर सकेगा। मन शान्त और मौन हो जायेगा उपवास से सभी रोग नष्ट किये जा सकते हैं। यदि कोई बहुत खाऊ व्यक्ति उपवास करने का विचार करे तो उसके लिए कठिनाई आयेगी। अल्पाहारी व्यक्ति को व्रत में सुख प्रतीन होगा। वह अधिक समय तक उपवास कर सकता है। दीर्घ काल तक निरन्तर उपवाम नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे किन्तु सतत अभ्यास करते रहना आवश्यक है। आरम्भ में मास में एक दिन का व्रत करें, फिर पन्द्रह दिन बाद और फिर धीरे-धीरे सप्ताह में एक बार उपवास करें।
१७८
गत आठ वर्षों से मैंने अपना समय विचारसागर, पंचदशी, गीता, उपनिषद् इत्यादि के स्वाध्याय में व्यतीत किया है और एक प्रकार से मैंने इन पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लिया है। किन्तु मुझे सबमें एकत्व होने की अनुभूति नहीं होती। क्या ग्रन्थ केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र के लिए हैं?
विचारसागर अथवा पंचदशी का अध्ययन मात्र करने से शुद्ध वेदान्तिक चैतन्य की अनुभूति नहीं हो सकती। वेदान्तिक तर्क-वितर्क अथवा शुष्क परिचर्चाएँ शास्त्रों की कर लेने से व्यक्ति को जीवन के एकत्व की अनुभूति में सहायता नहीं मिल सकती। आपको सभी प्रकार की अशुद्धियों, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, स्वयं के श्रेष्ठ होने की भावना इत्यादि जो मानव को मानव से अलग करने वाले बन्धक तत्त्व हैं, को कठोरतापूर्वक कुचलना पड़ेगा। यह सब शुद्ध भावना सहित निरन्तर मानवता की निष्काम सेवा करने से हो सकता है। आजकल व्यावहारिक वेदान्त दुर्लभ हो गया है। हर ओर शुष्क वाद-विवाद और धर्मों के अनावश्यक पहलू पर निरर्थक कलह दिखायी देते हैं। लोग गिनती की कुछ पुस्तकें पढ़ कर जीवन्मुक्त हो जाने का ढोंग करते हैं। यदि कहीं एक भी वास्तविक जीवन्मुक्त हो तो वह समस्त संसार को निर्देशित करने के लिए एक महान् सक्रिय शक्ति होगा। वह संसार का भविष्य परिवर्तित कर सकता है। आजकल के जीवन्मुक्त तो ग्रन्थ-कीट मात्र ही हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि थोड़ा सा लघुसिद्धान्तकौमुदी और तर्क का अध्ययन कर लेने से वे जीवन्मुक्त बन सकते हैं। जीवन का एकत्व तो केवल आत्म-साक्षात्कार से ही हो सकता है, और यह सतत आध्यात्मिक साधना करने से होगा। सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय थोड़ा सहायक होगा, किन्तु यह आपको जीवन्मुक्त नहीं बना सकता।
१७९
बहुत भलीभाँति ढूँढ़ने पर भी मैं सच्चा गुरु नहीं खोज पाया हूँ। क्या आप कोई बता सकते हैं?
ऐसा सच्चा गुरु खोज पाना जो शिष्य का गम्भीरतापूर्वक ध्यान रख सके, इस संसार में बहुत कठिन कार्य है, यह बिलकुल ठीक है। किन्तु एक ऐसा सच्चा शिष्य जो गम्भीरता से गुरु के निर्देशों का पालन करे, खोज सकना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। क्या आपने इस पहलू पर कभी सोचा है? गुरु के चयन में अपनी तर्क-शक्ति का बहुत अधिक उपयोग न करें। यदि आप प्रथम श्रेणी का गुरु खोजने में असफल हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति देखने का प्रयास करें जो गत कुछ वर्षों से आध्यात्मिक पथ पर चल रहा हो, जो सचरित्र हो तथा अन्य सद्गुणों से सम्पन्न हो, और जिसे सद्मन्थों का कुछ ज्ञान हो। जिस प्रकार जब सिविल सर्जन नहीं होता तो उसका छोटा असिस्टेंट रोगी की देख-रेख का कार्य सँभाल लेता है, उसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के स्तर का गुरु भी प्रथम श्रेणी के स्तर बाले गुरु के अभाव में बहुत सहायता कर देगा।
१८०
क्या संन्यासी के लिए भगवा रंग के वस्त्र पहनना अनिवार्य है?
संन्यासी की महिमा और उन्मुक्त स्थिति की कल्पना कर सकना गृहस्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। यदि अन्तर्मन में परिवर्तन हो, तो बाह्य रूप में भी परिवर्तन होना अति आवश्यक है। जिसके मन में परिवर्तन आ गया हो, उसके लिए भगवा वस्त्र अथवा गेरुआ वस्त्र धारण करना आवश्यक है। माया अथवा स्वभाववश जब इन्द्रियाँ भोग-पदार्थों की ओर जाने लगती हैं तो जैसे ही आपकी अपने पहने हुए वस्त्रों के रंग पर दृष्टि जाती है तो स्मरण दिला देती है कि आप संन्यासी हैं। यह आपको तुरन्त झटका दे कर गलत कार्य करने से बचा देती है। इस रंग की अपनी महिमा और अपने लाभ हैं। एक सच्चा सन्यार्थ ही समस्त सम्बन्धों और बन्धनों को काट कर मोह से छूट सकता है। उसके पुराने फिक और सम्बन्धी उसे परेशान नहीं करेंगे। जब व्यक्ति प्रवचन देने जाता है, तब भी यह पोशाक बहुत सहायता करती है। हिन्दू लोगों के मन में इस रंग के सम्बन्ध में एक अला प्रकार की पवित्रता का भाव है। सामान्य लोग संन्यासी के वचनों को अधिक सहजता मान लेते हैं।
१८१
आपने अपनी पुस्तक 'ईज़ी स्टैप्स टू योगा' में ब्रह्मचर्य के महत्त्व के विषय में कहा है। दिनभर के कठोर परिश्रम के बाद में अत्यन्त थक जाता हूँ। क्या अपनी उस धर्मपत्नी की ओर देखना पाप है जो मुझे सुख देती है? क्या ब्रह्मचर्य का पालन वृद्धावस्था से बचा देता है? रतिक्रीड़ा जीवन में पुनः नवीनता देने के लिए आवश्यक है। मनुष्य की समस्त मानसिक शक्तियाँ उसे समय से सम्बन्धित जन्म, आयु, वृद्धावस्था और मृत्यु की प्रक्रिया से बचा नहीं सकतीं। वंशवृद्धि हेतु स्त्री-पुरुष को यह रचनात्मक शक्ति प्रदान की गयी है। अतः क्या सम्भोग क्रिया इसके लिए आवश्यक नहीं है?
आपने विषय को पूर्णतया गलत दृष्टिकोण से देखा है। आपके सिद्धान्त की भूमिका ही पूरी तरह से गलत है। मोक्ष का भौतिक शरीर से सम्बन्ध नहीं है। एक बार जिसका जन्म हो गया, उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात् भौतिक शरीर की मृत्यु निश्चित है। वह अवस्था अमरत्व अथवा मोक्ष की अवस्था कहलाती है जिसमें आप जन्म-मरण के चक्र में प्रवेश किये बिना स्वतन्त्रता सहित निरन्तर आनन्द में विचरण करते हैं। जब तक आप स्वयं की उस परम तत्त्व के साथ एकत्व एवं पहचान को स्थापित नहीं कर लेते, जो देश-काल की समस्त सीमाओं से परे है, तब तक मोक्ष का आनन्द प्राप्त नहीं कर सकते। शाश्वत तत्त्व, परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने और उनका साक्षात्कार करने के लिए आपको अपनी शक्तियों का एक-एक कण अपने भीतर सँजो कर रखना चाहिए। वस्तुत हमारे भीतर केवल एक शक्ति है जो विविध रूपों में विभिन्न कार्य करती है। जिस प्रकार एक मशीन से लम्बे समय तक काम लेते रहने के लिए आप उसे बिना जंग लगने दिथे अथवा व्यर्थ के कार्यों में उपयोग न करते हुए यथोचित काम ही लेते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर को भी सही रूप में देख-रेख करते हुए दीर्घ आयु के लिए इसकी क्षमताओं एवं शक्ति को संचित रखना चाहिए। शरीर न रहने पर आप उच्चतर लोकों का कैसे अन्वेषण कर सकते हैं?
कृपया मेरे द्वारा अनूदित भगवद्गीता का अध्ययन करें। उसमें वर्णन किये गये त्याग का अभ्यास करें। यह आपको परिवार का त्याग कर देने के लिए नहीं कहता। अत्यका संसार में रहते हुए, संसार के द्वारा ही, संसार में आसक्ति न रखना सीखना पड़ेगा। आपको कर्तव्य, गृहस्थी में आसक्त न हो कर गृहस्थी चलाना है। केवल तब ही आपको मन की ऐसी पवित्रता प्राप्त होगी जो आपको असीम शान्ति, सुख और आनन्द के पथ पर उन्नति करने की योग्यता प्रदान करेगी। अपनी गलत धारणाओं की पालना
बहुत हो चुकी। अब जाग जायें और अपने वास्तविक अनश्वर रूप को जानें। अपने सच्चे, अमर, सर्वव्यापक आत्म-स्वरूप को देखें और अमरत्व के पावन अमृत का रसपान करते हुए उसमें स्थित हो जायें। मेरी शिक्षाओं के अनुसार चलें। आप पूर्णतया परिवर्तित व्यक्तित्व से सम्पन्न, आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति से सक्षम व्यक्ति बन जायेंगे। विश्वास रखें और गम्भीरता विकसित करें। सफलता आपकी होगी। आप ही 'वह' हैं। तत् त्वम् असि !
१८२
क्या आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्मयोग अनिवार्य है? यदि ऐसा है तो उसे कैसे करना चाहिए?
हाँ, निश्चित रूप से! यदि आप अपने मन की मलिनताओं को दूर करने के लिए निष्काम कर्मयोग के अभ्यास की उपेक्षा करते हैं तो आप वेदान्त के उद्देश्य और भाव को समझ और आत्मसात् नहीं कर सकते। निष्काम कर्मयोग से चित्त-शुद्धि प्राप्त होती है और अन्ततोगत्वा परमात्मा में एकत्व से साक्षात्कार तक पहुँचा देता है।
प्रत्येक व्यक्ति की गहन प्रेम से, 'मैं कर रहा हूँ' का भाव न रखते हुए, बिना फल की आशा से, परिणाम में कुछ प्राप्ति की इच्छा अथवा प्रशंसा प्राप्त करने तक की भी इच्छा न रखते हुए सेवा करें। यह अनुभव करें कि आप केवल एक निमित्त मात्र अथवा भगवान् के हाथों के उपकरण हैं। निर्धनों और रोगियों में भगवान् को देखते हुए, उनकी पूजा की भावना से सेवा करें। किसी भी स्थान, व्यक्ति अथवा वस्तु में आसक्ति न रखें। सफलता अथवा असफलता, लाभ अथवा हानि, सुख और दुःख की ओर ध्यान न देते हुए, संसार की इन समस्त परिवर्तनशील परिस्थितियों के मध्य में मानसिक सन्तुलन बनाये रखें। समस्त क्रियाशीलता में संलग्न रहते हुए मन को सदैव परमात्मा में सुस्थिा रखें। तब आप वास्तविक कर्मयोगी बन जायेंगे। सही भावना से किया गया कर्म, व्यकि को उन्नत करता है। यदि लोग आपका उपहास अथवा निन्दा करें, चोट पहुँचायें और मार भी डालें, तो भी तटस्थता बनाये रखें। अपनी साधना में लगे रहें।
१८३
मेरे जीवन में मेरी गलतियाँ और पाप असंख्य हैं और मेरा अज्ञान असीम है। संस्कृत भी मैंने सीखी नहीं। कृपया मुझे बतायें कि क्या आध्यात्मिक पश्थ पर मेरे चल सकने की कुछ सम्भावना है ?
अज्ञान तो एक मानसिक कल्पना है। 'आप' ज्ञान का साकार स्वरूप हैं। जब आवरण हट जाता है तो आप अपने निज स्वरूप में प्रकाशित हो जाते हैं। वासनाओं और अहंकार को निकल जाने दें। बादलों का छेदन कर दें। इन बादलों के पीछे उज्ज्वल सूर्य है। मन के पीछे स्व-प्रकाशित आत्मा है। स्वयं को शुद्ध करें। कुवृत्तियों को नष्ट कर डालें। आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ हो जायें। आपका जन्म केवल इसी के लिए हुआ है। आत्म-साक्षात्कार और आध्यात्मिक मार्ग के लिए संस्कृत जानना आवश्यक नहीं है। आपने केवल सिद्धान्त और सार को समझना है। सभी संस्कृत की पुस्तकें अँगरेजी तथा अन्य भाषाओं में उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में चिन्ता न करें। संस्कृत आपको थोड़ी सी सहायता कर सकती है, बस केवल इतना ही है। यदि आपके पास समय हो तो उसकी वर्णमाला सीख लें जिससे कि गीता के और उपनिषदों के कुछ स्तोत्र एवं श्लोक पढ़ सकें।
१८४
हम फल और सब्जियों को भी काटते हैं, क्या उसे हिंसा नहीं माना जाना चाहिए?
सब्जी और फलों को काटना हिंसा नहीं है। पौधों और वृक्षों में वास्तविक चेतना नहीं होती, यद्यपि जीवन उनमें भी है। पौधों में जीवन है, जानवरों में संवेदन-शक्ति है. मनुष्यों में मानसिकता है और सन्तों में आध्यात्मिकता है। पेड़-पौधों में विशेष अहकार और चैतन्य प्रतिबिम्बित नहीं है; अतः उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता। वृक्ष यह नहीं कहेंगे कि मुझे कष्ट हो रहा है। पेड़-पौधों में मन का विकास नहीं होता। यह बिलकुल प्रारम्भिक स्थिति में तथा अल्पवर्धित अवस्था में हैं। यह जड़ अथवा संज्ञाहीन हैं। यदि हम फल-सब्जियों को काटने में भी हिंसा देखेंगे तो पृथ्वी पर जीवन असम्भव हो जायेगा। यह तो केवल बाल की खाल निकालने वाली बात है। यह तो उन लोगों का निरर्थक दार्शनिक विचार है जो व्यर्थ के तर्क-वितर्क में लगे रहते हैं। ऐसे नगण्य विचारों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। व्यावहारिक व्यक्ति बनें।
१८५
भगवान् मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या बाधा है?
आत्म-समर्पण पूरी तरह से नहीं हुआ है। अभी भी सूक्ष्म मोह, सूक्ष्म इच्छाएँ और अति सूक्ष्म अहंभाव विद्यमान हैं। इन्द्रियाँ अभी अति बलवती एवं बाह्यगामी हैं। यह सब बाधाएँ हैं। जब यह दूर हो जायेंगी, तब आप अपने अन्तरतम में भगवान् की मधुर आवाज़ स्पष्ट सुन लेंगे। अशुद्ध प्राणी प्रायः अपने अशुद्ध मन की आवाज को भगवान् की आवाज समझने की गलती कर बैठते हैं।
१८६
मुझे इस झूठे संसार से घृणा हो चुकी है। मैं भलीभाँति जान गया हूँ कि ऐसे जगत् में रहने का कोई लाभ नहीं है। हर ओर केवल दुःख-कष्ट ही देखने में आते हैं। मैं संन्यासी जीवन जीना चाहता हूँ; किन्तु गुरु को कहाँ खोजूँ, यह नहीं जानता। कृपया मुझे बतायें कि संन्यासी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा ?
आपको संसार से नहीं, सांसारिक जीवन से घृणा करनी चाहिए। संसार तो भगवान् का प्रकटित स्वरूप है। संसार आपका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आपके कैवल्य प्राप्ति के मार्ग में यह संसार बाधा नहीं बन सकता। आपको ही अपना जीवन जीने का ढंग और वस्तु-पदार्थों को देखने का ढंग परिवर्तित करना होगा। आपको निश्चित रूप से नयी मानसिकता और नया दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। तब यही संसार स्वर्ग प्रतीत होगा। आपमें सच्चा वैराग्य अभी विकसित नहीं हुआ है। यह तो किसी दुःखद घटना या परिस्थितिवश उत्पन्न होने वाली क्षणिक अरुचि है। आप संन्यास लेने के अभी उपयुक्त नहीं हैं। सन्यासी के कर्तव्य निभाने में आप असफल हो सकते हैं। आध्यात्मिक सोपान की आपको एक-एक सीढ़ी पर क्रमानुसार चढ़ना पड़ेगा।
मैं आपको संसार में ही रहते हुए अपने चित्त की शुद्धि के लिए कुछ वर्षों तक निष्काम कर्मयोग करने का परामर्श देता हूँ। आपको विनम्रता, आत्म-त्याग, क्षमा, दया और विश्व-प्रेम की भावना स्वयं में विकसित करनी होगी। यह सद्गुण केवल निष्काम सेवा से ही अर्जित किये जा सकते हैं। आपमें संन्यास हेतु गुरु के पास पहुँचने से पहले निश्चित रूप से शम, दम, सर्व-संग-परित्याग और गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास एवं परिपूर्ण आज्ञाकारिता होनी चाहिए, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं होगा।
१८७
जब मैं यह जानती हूँ कि यह संसार सत्य नहीं है और मुझे एक-न-एक दिन छोड़ कर जाना ही होगा, तो इसे मैं अभी से ही क्यों न त्याग दूँ? पति-सेवा को अपना कर्तव्य समझते हुए मैं इसे बहुत सच्चाई और गम्भीरता सहित कर रही हूँ। किन्तु मैं जानती हूँ कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में न पति, न पुत्र, न पिता और न ही माता मेरी सहायता कर सकते हैं। मीराबाई ने क्या अपने पति को छोड़ देने पर ही भगवान् को प्राप्त नहीं किया था?
स्त्री के लिए उसका पति भगवान् का स्वरूप है। उसे केवल उसी में और उसी के माध्यम से भगवान् का साक्षात्कार करना होगा। उसे तो पूजा के लिए मन्दिर में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका वैराग्य क्षणिक उद्गार है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति में यह किसी भी प्रकार से आपका सहायक नहीं हो सकता। आप कहने को भले ही कह दें कि 'यह संसार सत्य नहीं है,' किन्तु आप अन्तर्मन से न जाने कितनी वस्तुओं में आसक्त होंगी। जो वैराग्य पारिवारिक कठिनाइयों और विपत्तियों से थोड़े से समय के लिए आता है, वह विद्युत् की चमक की भाँति होता है। झट से ही यह चला भी जाता है।
संसार किस प्रकार से असत्य है? संसार इस प्रकार असत्य नहीं है जैसे खरगोश के सींग अथवा बाँझ नारी का पुत्र। यह संसार सापेक्ष सत्य अर्थात् व्यावहारिक सत्ता है। यह ब्रह्म के समान सत्य नहीं है। जब ब्रह्म अथवा शाश्वत सत्य के साथ तुलना की जाती है तो इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। यह जगत् प्रातिभासिक अथवा प्रतीति है। ब्रहा परासत्ता अथवा परिपूर्ण सत्य है। जगत् केवल उस ज्ञानी के लिए असत्य है जो अपने निज स्वरूप में स्थित है। अधिकांश लोग 'मिथ्या' शब्द का सही रूप में अर्थ नहीं समझते। अतः वह बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी अनुशासन के और बिना किसी भी सद्गुण को उपार्जित किये ही संसार का त्याग करने का प्रयत्न करते हैं। यह शोचनीय भूल है। संसार को मात्र प्रतीति मान कर, आपको संसार में अधक धैर्य से, अहंकारशून्य हो कर, आत्मभाव सहित परम सत्ता के अथवा जगत् के मूल आधार के सुस्पष्ट ज्ञान के साथ कार्य करना होगा। यदि साधक निष्काम कर्मयोग के द्वारा हृदय को शुद्ध किये बिना तथा मोक्ष-प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन-चतुष्टय को अर्जित किये बिना संसार का त्याग करता है तो ऐसे त्याग से उसे किंचित् भी लाभ नहीं होगा।
मीरा की बात बिलकुल अलग थी। वह परिपूर्ण वैराग्य सम्पन्न तथा बाल्यावस्था से ही कृष्ण-प्रेम से परिपूरित हृदय से सम्पन्न थी। आपकी बात अलग है। अतः यह तुलना न करें। आपको अपनों की और मानवता की सेवा के द्वारा स्वयं को विकसित करना होगा। इसका अभ्यास करें। अपने पति के उज्ज्वल नेत्रों में और सभी के चेहरों में भगवान् कृष्ण के दर्शन करें। भगवान् की कृपा आप पर हो!
१८८
अभी मेरे मन में गृहस्थ-जीवन को त्यागने की कोई इच्छा नहीं है और फिर भी कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत करने की मुझे तीव्र इच्छा है। क्या यह सम्भव है? क्या श्रद्धेय आपश्री मेरी सहायता करेंगे ?
हाँ, आप गृहस्थ-आश्रम में रह सकते हैं। किन्तु आदर्श गृहस्थ बन कर रहें। अन्य तीनों आश्रमों का पोषण करें। यदि गृहस्थी के कर्तव्यों का नियम-निष्ठा से पालन किया जाता है तो संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है।
पूर्ण रूप से सत्य-निष्ठ ब्रह्मचारी बन जायें और मैथुन क्रिया का सर्वथा त्याग कर दें। आप पर्याप्त सन्तान प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप वास्तविक, ठोस, तीव्रगामी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो योगाभ्यास की यह अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। अपनी धर्मपत्नी को भी आध्यात्मिक मार्ग पर प्रशिक्षित करें। वह भी उसी मन्त्र का जप करे जिसका आप कर रहे हैं और धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय तथा समय-समय पर उपवास करे अथवा दूध-फल का आहार ले।
शीर्षासन आप करते रह सकते हैं। सही आचरण के नियमों का कठोरता से पालन करें। यम-नियमों के अभ्यास में स्थिर हो जायें। कुण्डलिनी जाग्रत करने से पहले अपने हृदय को पवित्र बनायें। ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग और द्वेष से स्वयं को पूर्णतया मुक्त करें। तब कुण्डलिनी अत्यन्त सरलता से जागृत हो जायेगी। इसे जगाने में, मैं आपकी सहायता करूँगा। चिन्ता न करें। अपना जप और ध्यान बढ़ा दें। गृहस्थ रहते हुए ही आप आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु काया, वाचा, मनसा ब्रह्मचारी होना आपके लिए नितान्त आवश्यक है।
१८९
श्रद्धेय स्वामी जी, आपनी ने मनुष्य को पुत्र का पिता बनते ही अपनी धर्मपत्नी को 'विश्वमाता' की दृष्टि से देखने का उपदेश दिया है। किन्तु यदि जन्म के कुछ मास पश्चात् पुत्र का देहान्त हो जाये तो उसकी स्थिर सम्पत्ति की देख-रेख के लिए उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कृपया मुझे अपना परामर्श दें।
अपनी स्थिर सम्पत्ति की आप क्यों चिन्ता करते हैं? क्या यह सम्पत्ति आप अपने साथ ले कर आये थे? और क्या मृत्यु के साथ ही आप इसे अपने साथ ले कर जायेंगे? धन-सम्पदा अथवा अचल सम्पत्ति है क्या? धरती का केवल एक छोटा टुकड़ा ही तो है न? क्या जमीन-जायदाद और उसका उत्तराधिकारी आपको सुख और शान्ति दे सकते हैं? क्या यह सब दुःख-चिन्ता के साधन और कारण नहीं हैं? धन-सम्पत्ति और सन्तान की इच्छा मनुष्य को संसार-चक्र से बाँध देती है। जिज्ञासु साधक के लिए यह सब बाधाएँ हैं।
भगवान् बुद्ध और भर्तृहरि ने अपनी धन-सम्पत्ति का क्या किया था ? क्या उनमें से किसी ने भी उसकी देख-रेख के लिए पुत्र-प्राप्ति की लालसा की? जो व्यक्ति धन, गृह एवं पुत्र की चिन्ता करता है, वह भगवान् का चिन्तन कैसे कर सकता है? भगवान् और धनपरायणता दोनों का एक-साथ चिन्तन असम्भव है। प्रकाश की उपस्थिति में अन्धकार नहीं ठहर सकता। जब तक आप विषय-पदार्थों को भोगने में सुख मानते रहेंगे तब तक आत्मा का आनन्द अनुभव नहीं कर सकते।
यदि आपको अन्य और पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो अपने कष्टों में और वृद्धि कर लेंगे। पहले ही आपके कण्ठ में बहुत से बन्धन पड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया है कि मानव के क्लेश कितने अधिक हैं, वह कभी भी सन्तान को जन्म दे कर संसार में नहीं लायेगा। यदि आपका मन वासनाओं से भरा हुआ है और यदि आपको इन वासनाओं को नष्ट करना कठिन लगता है, तो आप दूसरा पुत्र प्राप्त कर लें और उसके बाद पूर्ण ब्रह्मचारी बन जायें।
१९०
भगवान् सर्वव्यापक एवं निराकार हैं। उन्हें मूर्ति में सीमित कैसे किया जा सकता है? मूर्तिपूजा का क्या लाभ है?
सर्वव्यापक भगवान् की दिव्यता सृष्टि के प्रत्येक कण में स्पन्दित है। विश्व-ब्रह्माण्ड में एक कण भी ऐसा नहीं है जहाँ वह नहीं है। तब फिर आप यह क्यों कहते हैं कि वह मूर्ति में नहीं हैं?
नये साधकों के लिए मूर्ति एक आधार है। यह उसके आध्यात्मिक बचपन का अवलम्बन है। प्रारम्भ में आकार अथवा मूर्ति, पूजा के लिए आवश्यक है। अनन्त के ऊपर, निराकार परम सत्ता पर मन को केन्द्रित कर सकना सबके लिए सम्भव नहीं होता। ध्यान का अभ्यास करने के लिए अधिकांश साधकों को किसी ठोस आकार की आवश्यकता होती है।
मूर्तियाँ मूर्तिकारों की निरर्थक कल्पनाएँ नहीं हैं, अपितु ऐसी उज्ज्वल प्रणालियाँ हैं जिनके माध्यम से भक्त के हृदय की संवेदनाएँ भगवान् की ओर प्रवाहित होती हैं। यद्यपि पूजा मूर्ति की की जाती है, किन्तु भक्त उसमें भगवान् की विद्यमानता को अनुभव करता है और अपनी सम्पूर्ण भक्ति-भावना उसमें समाहित कर देता है। मूर्ति तो मूर्ति ही रहती है, किन्तु उपासक की पूजा उसके भगवान् तक पहुँच जाती है।
भक्त के लिए मूर्ति अथवा चित्र चैतन्य का पुंज होता है। वह मूर्ति से प्रेरणा प्राप्त करता है। मूर्ति उसका निर्देशन करती है। उससे वार्तालाप करती है। यह मनुष्य का रूप धारण करके अनेक प्रकार से उसकी सहायता करती है। दक्षिण भारत के मदुरै मन्दिर के भगवान् शिव की मूर्ति ने मनुष्य रूप से एक लकड़हारे और एक वृद्धा की सहायता की। तिरुपति मन्दिर की मूर्ति ने मनुष्य का रूप धर कर अपने भक्त की सहायतार्थ न्यायालय में गवाही दी थी। ऐसे कितने ही चमत्कार और रहस्यमय उदाहरण हैं।
केवल हिन्दू धर्म में ही मूर्तिपूजा नहीं है। ईसाई क्रॉस को पूजते हैं। उनके मन में क्रॉस की छवि रहती है। मोहम्मदी काबा की शिला का ध्यान मन में रख कर प्रार्थनाएं करते हैं। मानसिक प्रतिबिम्ब भी मूर्ति का रूप है। यह केवल स्तर का ही अन्तर है, बात तो एक ही है।
सभी उपासक भले ही कितने भी बुद्धिवादी क्यों न हों, अपने मन में एक आकार बना लेते हैं और मन को उस पर केन्द्रित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मूर्तिपूजक है। चित्र और छवि भी केवल प्रतिमा का ही रूप हैं। स्थूल मन के अवलम्बन के लिए स्थूल प्रतीक की आवश्यकता होती है तो सूक्ष्म मन को सूक्ष्म आधार की। वेदान्ती के लिए भी चचल मन को स्थिर करने के लिए ॐ का प्रतीक होता है। केवल चित्र अथवा पत्थर या लकड़ी की प्रतिमा ही मूर्ति नहीं है। अक्षर और सांकेतिक बिन्दु भी मूर्ति बन जाते हैं। अतः मूर्तिपूजा को दोष क्यों देना ?
१९१
क्या नारी केवल पुरुष के लिए, उसकी सेवा करने के लिए ही बनायी गयी है? क्या भगवान् ने हमें केवल रसोईघर के और सन्तानोत्पत्ति के लिए ही बनाया है ? स्त्री गौण भूमिका क्यों निभाये ? नारी को समानाधिकार देना क्यों नहीं चाहते आप ?
स्त्री किसी भी प्रकार से पुरुष से निम्न नहीं है। गृह एक सहयोगी संस्था है। यह कार्य-विभाजन के सिद्धान्त पर उन्नत होती है। यदि पुरुष धनोपार्जन करता है और त्वी घर में रहती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री पराश्रयी अथवा दासी है। वस्तुतः वह राष्ट्र की निर्माता है। एक महिला का अपनी सन्तान को प्रशिक्षित करके उत्तम नागरिक बनाना तथा इस प्रकार समस्त मानव-जाति का चरित्र निर्माण करना निःसन्देह उससे कहीं अधिक एवं श्रेष्ठतर शक्ति एवं सामर्थ्य होने का परिचायक है जो कि वह निर्णायक अथवा विधायक या अध्यक्ष अथवा मन्त्री या न्यायाधीश बन कर प्राप्त करने की आशा रखती है।
यह विचारधारा कि स्त्री और पुरुष समान हैं, वस्तुतः पश्चिम की धारणा है। भारतीय अथवा हिन्दू धारणा के अनुसार पुरुष और स्त्री, पुरुष और शक्ति एक एवं अविभाज्य हैं। सीता ने स्वयं का भिन्न अस्तित्व नहीं समझा। वह श्री राम में ही थीं, और राम की ही थीं। भारतीय नारी सदैव प्रत्येक पारिवारिक, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में अपना तादात्म्य पूर्णतया अपने पति के साथ ही बनाये रखती है। वह अपने गृह की साम्राज्ञी है। मातृत्व की महिमा से वह अपने गृह को प्रकाशित करती है। मातृत्व में ही नारी का समस्त विशेषाधिकार, उसकी महिमा, योग्यता और उसका अधिकार-क्षेत्र विशेष रूप से निहित है।
पश्चिमी जगत् ने महिलाओं को पुरुषों के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेते हुए देख लिया है। किन्तु मैं पूछता हूँ: "इससे क्या उन देशों में मानव जीवन में अधिक प्रसन्नता और देश की समृद्धि एवं शान्ति में अधिक वृद्धि हो गयी है? हाँ, इससे अधिक तलाक, अधिक क्लेश, अधिक व्याकुलता ही बढ़ी है। इसने केवल स्त्रियों के अज्ञान के आवरण को घनीभूत तथा उनमें राजसिक तत्त्व का संवर्धन अवश्य ही कर दिया है।"
पश्चिमी जगत् में भी बहुत से व्यक्ति हैं जो स्त्रियों की पुरुषों के साथ समानाधिकार की माँग के पक्ष में नहीं हैं। जो इस धारा के पक्ष में थे, वह भी अब अपने इस गलत समर्थन के लिए गम्भीरतापूर्वक पश्चात्ताप कर रहे हैं, क्योंकि वे वस्तुतः अपनी दृष्टि के समक्ष इसके दुष्परिणाम देख रहे हैं।
स्वच्छन्द जीवन, परिपूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होती। संयमविहीन मिलना-जुलना स्वतन्त्रता नहीं है। इस झूठी स्वतन्त्रता में पड़ कर कई भारतीय महिलाओं ने अपना जीवन स्वयं ही नष्ट कर लिया है।
पश्चिमी जगत् की नारी का आदर्श हमारा आदर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हम केवल अप्राकृतिक ही नहीं अपितु अराष्ट्रिय भी हो जायेंगे। एक राष्ट्र अन्य किसी देश के आदर्श तथा सामाजिक प्रथाओं को, स्वयं अपनी आधारभूत संस्कृति को समझे बिना, नहीं अपना सकता।
महिलाओं को केवल श्रेष्ठ माताएँ बनना चाहिए। भगवान् की भव्य योजना में उन्होंने ही यह कार्य करना है। दिव्य योजना का तात्पर्य यही है। भगवान् की इच्छा यह ही है। नारी के अपने विशेष मनोवैज्ञानिक गुण, स्वभाव, योग्यताएँ, वृत्तियाँ और मनोभावनाएँ हैं। समाज में उनकी कुछ अपनी अक्षमताएँ अथवा सीमाएँ हैं। वे पुरुषों के साथ अपनी तुलना न कर सकती हैं, न ही करनी चाहिए।
१९२
क्या वैवाहिक जीवन ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्ति में बाधक नहीं है? एक विवाहित व्यक्ति एक-साथ परमात्मा और अपनी पत्नी को कैसे प्रसन्न कर सकता है?
वे लोग जो सांसारिक वस्तु-पदार्थों के प्रति त्याग एवं अनासक्ति की भावना से सम्पन्न हैं तथा जो यह समझते हैं कि जीवन की प्राप्ति प्रकृति रूपी महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके स्वयं को सही साँचे में ढालने के लिए ही हुई है, उनके लिए वैवाहिक जीवन कभी भी बाधक नहीं बन सकता। त्यागराज, एकनाथ, नरसी मेहता, भद्राचलम् रामदाम, तुकाराम, नामदेव, जयदेव, चैतन्य और कबीर जैसे सन्तों के जीवन-चरित पढ़ें। संसार में गहरे उतर कर देखें और उस मार्ग को, उस पथ को देखें जिसका अनुसरण ऊपर बताये सन्तों, भक्तों ने तथा उनके जैसे अन्य अनेकों ने करते हुए जीवन व्यतीत किया।
मनुष्य यदि अपनी पत्नी को अपनी प्रसन्नता के साधन के रूप में प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो यह उसके लिए लज्जास्पद है। जो व्यक्ति यह समझता है कि वैवाहिक जीवन का उद्देश्य पत्नी को प्रसन्न करना मात्र ही है, वह तो एक अधम दास से भी होन है। आत्म-संयमी बनें। अपनी धर्मपत्नी को भी जीवन के उद्देश्य तथा उस उद्देश्य को गृहस्थ-जीवन के माध्यम से प्राप्त करने के साधन के प्रति जागरूक करें। अपनी निम्न प्रवृत्तियों के हठी स्वभाव अथवा आपके जीवन-साथी के निम्न हठ के समक्ष मत चुके, अपितु स्वयं को सन्तुलित ढंग से इस प्रकार सुनियोजित कर लें कि आप दोनों में से किसी की भी शारीरिक एवं मानसिक अवस्था अव्यवस्थित न हो। आप जो भी कुछ करें, उसे अपना न समझते हुए भगवान् को समर्पित कर दें। आत्म-शुद्धि-युक्त सन्तुष्ट एवं संयमो जीवन के लिए प्रार्थना करें। स्वयं को आध्यात्मिक युद्धभूमि में बिना सोचे छोड़ दें और फिर पीछे न पलटें, भले ही जीवन को दाँव पर क्यों न लगाना पड़े। अपने-आपके मालिक बनें और स्वयं को भगवान् का ही दास समझें, अपनी पत्नी का नहीं। आप अपने विवाहित साथी के साथ हैं इसका अभिनय भलीभाँति निभायें, किन्तु मानसिक दृष्टिकोण को सदैव इससे अतीत बनाये रखें। आप जीवन को सुरक्षित रूप से निभा सकेंगे।
१९३
क्या निर्गुण और सगुण दोनों भावों को बनाये रखने हेतु मैं 'ॐ' के स्थान पर 'ॐ नारायण' का जप करूँ ? नारायण मन्त्र का जप मेरे मानस-पटल पर भगवान् की चतुर्भुज मूर्ति बनाये रखता है। यद्यपि मुझे भगवान् श्री कृष्ण की मूर्ति पर ध्यान करने का अभ्यास बना हुआ है और मैं भगवान् श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप और उनके चरणों में बैठे हुए अर्जुन के चित्र की खोज में हूँ। कृपया मुझे बतायें कि भविष्य में मुझे क्या और कैसे करना चाहिए।
आपने पहले ही भगवान् श्री कृष्ण पर ध्यान करके उसके बल एवं शक्ति से सुस्पष्ट मानसिक छवि बना ली है। अब चयनित एवं निर्मित रूप में परिवर्तन करना अच्छा नहीं है। यदि आप परिवर्तित कर भी लेंगे तो भी स्वभाववश पुरानी छवि आपके समक्ष आती रहेगी। अतः उसी छवि को ही अपनाये रखें। चतुर्भुज भगवान् कृष्ण की छवि की खोज छोड़ दें।
'ॐ नारायण' सही मन्त्र नहीं है। सही मन्त्र है- 'ॐ नमो नारायणाय'। 'مق सगुण और निर्गुण दोनों ही है। यदि आप प्रश्नोपनिषद् का अध्ययन करें तो इस तथ्य को भली प्रकार से समझ जायेंगे।
यदि आप मन्त्र-परिवर्तन करना ही चाहते हैं तो आप 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप कर सकते हैं।
१९४
मैं उपनिषद् तथा अन्य ग्रन्थों का स्वाध्याय करता रहा हूँ और उनमें मैंने पाया है कि लगभग सभी में एक ही बात है। वह सब कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे सामने है, सब असत्य है, केवल भगवान् ही सत्य हैं और यह सत्य हमें स्वयं ही विचार करके समझना पड़ेगा। स्वामी जी, हम यह कैसे करें?
अध्ययन केवल कुछ सीमा तक ही सहायक होगा। अत्यधिक अध्ययन से आप भ्रमित हो जायेंगे। आपको एक निश्चित विचार पर एकाग्रित हो कर ध्यान करना चाहिए। वह निश्चित विशेष विचार आपके ज्ञान-चक्षु खोलने का कार्य करेगा। केवल तब ही आपमें वैराग्य-भाव आयेगा, आप वस्तु-पदार्थों की असत्यता को तब ही समझ सकेंगे। उदाहरण के लिए नेरुर के श्री स्वामी सदाशिव ब्रहोन्द्र के जीवन को लें। अपनी माँ को भोजन देने के लिए कहने पर, उनकी माँ के कहे गये केवल एक, 'प्रतीक्षा करो' शब्द ने उनके मन पर ऐसा प्रहार किया कि वे तुरन्त 'सत्य' को समझ गये।
आप बौद्धिक स्तर पर भले ही यह जानते-समझते हैं कि जगत् मिथ्या है, केवल परमात्मा ही वास्तविक हैं तथा समस्त विषय-भोग केवल दुःख का ही कारण हैं, किन्तु आपकी यह धारणा अभी सुदृढ़ नहीं है। आप सोचेंगे, "मैं केवल पाँच मिनट के लिए इन्द्रिय-विषयों का सुख ले लेता हूँ।" और इस प्रकार आप माया द्वारा छल लिये जायेंगे। सभी विषय-भोग माया द्वारा निर्मित चीनी में पगी गोलियाँ हैं। आपको 'ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते...' जैसे श्लोकों पर चिन्तन करना चाहिए। उच्चतर परम आत्मा, जो अनन्तता, शाश्वतता, असीमता है, के साथ आपको तादात्म्य स्थापित करना चाहिए। सदैव विचार करें, "शुद्धोऽहम्, शान्तोऽहम्, सच्चिदानन्दोऽहम्।" आप उन्नत भाव को प्राप्त करेंगे। अभ्यास एवं वैराग्य आवश्यक हैं। त्याग और तपस्या आपको अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान करेंगे। संसार के क्षणिक सुखों, मोटरगाड़ी, धन-सम्पत्ति के छल में न फँसें और अवांछित आसक्ति द्वारा व्यर्थ चिन्तित न रहे। अपने कर्तव्य करते जायें और शेष भगवान् पर छोड़ दें। वे आपकी रक्षा करेंगे।
१९५
क्या आत्म-साक्षात्कार प्राप्त सन्त स्वार्थी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने केवल अपने लिए ही मोक्ष की आकांक्षा रखी ? और फिर यदि सभी संन्यासी हो जायेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा ?
यह प्रश्न अनुचित कल्पना पर आधारित है। यदि सभी स्त्रियाँ बाँझ हो, यदि सभी चिकित्सक बन जायेंगे, वकील या डाकू बन जायेंगे तो संसार का क्या होगा? केवल कतिपय गिने-चुने आध्यात्मिक सम्पदा से सम्पन्न व्यक्ति ही वैराग्य और त्याग प्राप्त का सकते हैं।
सन्त समस्त संसार को पवित्र कर देता है। वह स्वार्थी नहीं होता। शंकर, रामानुज तथा अन्यों ने समस्त मानवता की सेवा की। यहाँ तक कि जो एकान्तवासी है अथवा जो अज्ञातवास में रहता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह भी अपनी विचार-संवेदनाओं को प्रवाहित करके संसार को प्रभावित करता है। एक नव-शिष्य तक भी आध्यात्मिक पथ पर चलता हुआ अपने पवित्र विचारों द्वारा संसार का भला करता है। यह सब बाते, सन्तो एवं सन्त-सुलभ लोगों के ढंगों तथा उनके कार्यों को अशुद्ध मन बाला व्यक्ति समझ नहाँ सकता।
१९६
ब्रह्मचर्य का पालन अर्थहीन ही प्रतीत होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में परीक्षणों के द्वारा सिद्ध कर दिया है कि वीर्य को शरीर-प्रणाली में पुनर्संयुक्त नहीं किया जा सकता और यह भी कि मस्तिष्क का वीर्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।
वीर्य एक रहस्यमय स्राव है जो जीवित शरीर की रचना करने में सक्षम है। वीर्य स्वयं में एक जीवन्त पदार्थ है। यह स्वयं ही जीवन है। इसलिए जब यह मनुष्य में से निकल जाता है तो यह उसके अपने जीवन का एक अंश ले जाता है। एक सजीव वस्तु को पहले निर्जीव किये बिना प्रयोगशाला के परीक्षणों में नहीं डाला जा सकता। वैज्ञानिकों के पास इसका परीक्षण करने के लिए कोई उपकरण नहीं है। भगवान् ने इसके मूल्यवान् गुण को सिद्ध करने के लिए केवल एक ही परीक्षण की रचना की है, वह है गर्भाशय। वीर्य जीवन की रचना कर सकता है, केवल एक यही तथ्य सिद्ध करता है कि यह स्वयं ही जीवन है।
मेरे पास ऐसे सहस्रों नवयुवकों के पत्र आये हुए हैं जिन्होंने इस बहुमूल्य द्रव्य को व्यर्थ नष्ट किया है और वह अब दुःखदायी स्थिति में हैं। बहुत से युवकों की तो दुर्दशा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वह आत्महत्या करने को तत्पर हो गये! वीर्य को निमर्मतापूर्वक नष्ट करके उन्होंने अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का विनाश कर लिया है। जो परिपूर्ण ब्रह्मचारी हैं उनके नेत्र उज्ज्वल, देह-मन सुदृढ़ एवं स्वस्थ तथा बुद्धि कुशाग्र होती है।
अपनी परीक्षण-नलिकाओं और तुलाओं के साथ वैज्ञानिक सूक्ष्म वस्तुओं की गहराई तक पहुँच नहीं सकते। शरीर की कितनी भी चीर-फाड़ करने से, आत्मा कहाँ है यह बताया नहीं जा सकता, जीवन कहाँ है अथवा मन कहाँ है यह जाना नहीं जा सकता। योगाभ्यास के द्वारा, वीर्य-शक्ति (यह स्थूल भौतिक वीर्य द्रव्य नहीं) ऊर्ध्वगमन करके मन को सम्पन्न एवं सक्षम बना देती है। यह सन्तों की उद्घोषणा है। इसका अनुभव आपको स्वयं करना होगा।
१९७
जिस मनुष्य को यह विश्वास हो जाये कि उसके लिए जीवन अब अर्थहीन हो गया है, उसके लिए क्या आत्महत्या का निर्णय कर लेना तर्कसंगत है ?
आत्महत्या, अर्थहीन जीवन का तर्कसंगत निर्णय नहीं है, अपितु यह एक ऐसे विचारहीन एवं विवेक रहित मन द्वारा निश्चित अतर्कपूर्ण निर्णय है जो जीवन में निहित अर्थ को देख सकने में असफल हो गया हो। आत्महत्या कष्टों को दूर एवं दोषों में सुधार नहीं करती, प्रत्युत् यह कालान्तर में उग्र प्रतिक्रियाओं की ओर अग्रसर करती है। और वह प्रतिक्रियाएँ अब के इस असन्तोषजनक जीवन की वर्तमान अवस्था से भी अधिक कष्टदायी होंगी। आत्महत्या पूर्णरूपेण पराजयवाद है।
१९८
यदि संसार से पलायन लक्ष्य हो तो समाज-सेवा के लिए प्रोत्साहन कहाँ रहा?
संसार से पलायन लक्ष्य नहीं है अपितु सांसारिकता से मुक्त होना वांछनीय है। जीवन के एक स्तर तक समाज-सेवा का अपना मूल्यवान् स्थान है, किन्तु समय के साथ व्यक्ति को अपनी उच्चतर चेतना द्वारा इसका अतिक्रमण करके इससे अतीत चले जाना होता है। तथापि समाज-सेवा का मूल्य पूर्णतया व्यक्तिपरक है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति महान् समाज-सुधारक अथवा मानवता का रक्षक अपने-आपको यों ही बना लेता है, अपितु ऐसा है कि वह अपने अहम् को विश्व-प्रेम की वेदिका पर बलिदान करता है और उससे मन की पवित्रता को प्राप्त करता है। यह पवित्रता ही समस्त आध्यात्मिक विकास का आधार है। किन्तु साक्षात्कार प्राप्त महात्मा के हृदय में अपने साथी प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना से सेवा-भावना स्वयमेव ही उत्पन्न होती है।
१९९
जीवन की समस्त परिस्थितियों में अविचल शान्ति एवं मन की स्थिरता को विकसित करने के क्या साधन हैं? क्या परिपूर्ण प्रशान्तावस्था को प्राप्त करना सम्भव है?
जी हाँ, बिलकुल सम्भव है। ऐसा समझें कि आप संसार के लिए मृत हैं अथवा संसार आपके लिए समाप्त हो चुका है। आत्म विचार शक्ति को विकसित करें। मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि अथवा मन की अन्य किसी भी प्रकार की वृत्ति से अपना 'मैं-पन' न जोड़ें। सदैव अपने-आपको दिव्य विचारों में संलग्न रखें। स्वयं अपने अथवा अपने आस-पास के संसार के सम्बन्ध में कुछ भी विचार मन में न आने दें। अपने चतुर्दिक् के बातावरण के प्रति, विभिन्न दैनिक घटनाओं के प्रति, सांसारिक प्रतिघातों के प्रति, और यहाँ तक की स्वयं अपने प्रति भी पूर्णतया उदासीन रहें। आत्मज्ञान की एक बार अनुभूति हो जाने पर व्यक्ति समस्त मानसिक विघटनों एवं विकृतियों से मुक्त हो जाता है। जहाँ आध्यात्मिक जिज्ञासु के भीतर आत्मज्ञान सुदृढ़तापूर्वक स्थिर हो, जहाँ उसमें यह चेतना पूर्णतया जागरूक हो कि, "सब-कुछ वस्तुतः ब्रह्म ही है, सर्व खल्विदं ब्रह्म," और कि वह परब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है, और जहाँ वह समझता हो कि समस्त घटनाएँ अच्छी, बुरी अथवा मिश्रित - संसार के चित्रपट पर परिवर्तित होने वाले दृश्य मात्र हैं, वहाँ कभी भी असन्तुलित मानसिक जीवन हो ही नहीं सकता।
यह मन ही बन्धन अथवा मोक्ष का एकमात्र कारण है। सुख हो अथवा दुःख, प्रसन्नता हो अथवा संकट, सफलता हो अथवा विफलता सबके पीछे आधार एकमात्र मन ही है। गुरु और उसकी शिक्षाओं की शरण में होते हुए द्वन्द्वों से ऊपर उठ कर उनसे अतीत चले जायें। उन सन्तों के जीवनचरितों का स्वाध्याय करें जिन्होंने विविध संघर्षों का सामना किया तथा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त महात्माओं की रचनाओं का अध्ययन करें। ऐसी सच्ची समर्पण-भावना को विकसित करें जिसमें आपको अपनी देह अथवा शारीरिक आवश्यकताओं का, अथवा आत्मरक्षा का विचार ही उत्पन्न न हो, जिसमें आपके जीवन और मृत्यु का विचार ही विस्मृत हो जाये। प्रशान्तता तो केवल मानसिक अवस्था है। अतः आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही मानसिक साम्यावस्था को विकसित करें।
२००
गंगा के पानी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसे सदा के लिए किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त समझने के धार्मिक अथवा वैज्ञानिक क्या कारण हैं?
क्या यह सत्य है कि गंगा में एक गोता लगाने से समस्त पाप धुल जाते हैं?
अनन्त काल से माँ गंगा का सम्बन्ध उन सन्त-महात्माओं से जुड़ा हुआ है जो इसके जल में स्नान करके अथवा इसका पान करके अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं।
अग्नि अन्य समस्त वस्तु-पदार्थों को जला सकती है, किन्तु स्वयं अपने को नहीं। हिमालय के उच्च शिखरों से प्रवाहित होने वाली गंगा माँ के जल में हिम-शिखरों पर होने वाली वह असंख्य अद्भुत जड़ी-बूटियाँ मिली होती हैं जिनमें उच्चतम स्तर के संक्रमणहारी शक्तियों से सम्पन्न रसायन अपनी शुद्धतम अवस्था में निहित रहते हैं। इसके कारण उसमें गिराये गये अन्य प्रदूषक पदार्थ अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। हमारे समस्त धार्मिक विश्वास सशक्त वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित हैं।
और हाँ, यदि आप मन में इस सच्ची भावना के साथ गंगा माँ में गोता लगाते हैं कि आप अपने अनुचित कर्मों के लिए प्रायश्चित्त करने के साथ-साथ पुनः न करने का निश्चय कर रहे हैं तो अवश्य ही समस्त पाप धुल जाते हैं।
२०१
क्या आप भी मेरे इस विचार से सहमत हैं कि समाज में खुले आम घूमने वाले नागा साधु हमारी संस्कृति के लिए संकटकारी हैं? क्या वे उस स्तर तक उन्नत हो चुके हैं कि नग्नता में कुछ भी असभ्यता अथवा अनौचित्य न मानें? क्या शरीर को पूरी तरह से नग्न रखने का कोई आध्यात्मिक महत्त्व वास्तव में है? कृपया प्रकाश डालें।
हमारी पावन संस्कृति निश्चित रूप से प्रत्येक दृष्टि से आध्यात्मिक है। केवल जब उसके अन्तर्निहित भाव को विस्मृत कर दिया जाता है तब ही शालीनता और अश्लीलता जैसी द्वन्द्वात्मकताएँ उत्पन्न होती हैं। यह सभी द्वन्द्व पूर्ण विचारों का केवल सांसारिक मनुष्य के लिए अस्तित्व है, उसके लिए नहीं जो उनसे अतीत जाने और स्वयं को उस अद्वैत, भेदभावहीन अवस्था में स्थित होने के लिए प्रयत्नशील है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से फिर आप द्वैत भाव को खोजने और उससे प्रभावित होने के निम्न स्तर तक कैसे उतर सकते हैं?
नग्न रहने का आध्यात्मिक महत्त्व देहात्म-बोध अथवा शरीर-अभिमान से ऊपर उठने में सहायक तत्व होने में निहित है। जिस व्यक्ति का मन सांसारिक विचारों से दूषित है और जो द्वैत भावना से पूर्ण है, वह स्वयं को जन्मकालीन पोशाक में जनता के सामने प्रस्तुत करने में लज्जा अनुभव करेगा। जिसने अपने मन और इन्द्रियों को जीत लिया है, केवल वही जनसाधारण के मध्य निर्भीक हो कर और किञ्चित् भी प्रभावित हुए बिना नग्नावस्था में विचरण कर सकता है।
कुछ लोग देहाभिमान से ऊपर उठने के लिए अपनी साधना के एक अंग के रूप में इसे अपना लेते हैं और ऐसे साधक प्रायः लोगों के मध्य आने से दूर रहते हैं। निःसन्देह, ऐसे लोग भी हैं जो साक्षात्कार प्राप्त सन्त होने का स्वाँग करते हैं और भोलेभाले लोगों को छलने के उद्देश्य से जनसाधारण के मध्य घूमते हैं। किन्तु ऐसे नकली सन्तों को, उनकी प्रतिक्रियाओं को देखने से ही लोग अत्यन्त सरलता से पहचान सकते हैं और उनसे दूर रह सकते हैं।
२०२
आप किस आधार पर मांसाहार का विरोध करते हैं?
चिकित्सीय, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर। हमारा मन हमारे द्वारा खाये जाने वाले आहार से बना है। तामसिक भोजन के परिणामस्वरूप मन तामसिक होता जाता है। मांसाहार तामसिक है, अतः इससे दूर रहना चाहिए।
जब पशु की हत्या की जाती है तो उसकी स्नायु प्रणाली में मृत्युभय के कारण संकुचन होता है (आपने भी भय की परिस्थिति में अपने आमाशय में उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की विचित्र असुविधा को अनुभव किया होगा)। इस भय के कारण उस पशु के यकृत इत्यादि भीतरी अंगों से कुछेक विषैले द्रवों का स्राव होता है। इन विषैले द्रवों का प्रभाव उसके मांस में मिल जाता है और वह पकाये जाने पर भी नष्ट नहीं होता। अतः आमिष-आहार कालान्तर में खाने वाले व्यक्ति के ऊपर विषैला और भयंकर प्रभाव डालता है।
यदि समस्त शरीरों के भीतर निवास करने वाली आत्मा की दृष्टि से देखें तो आपमें और पशुओं में कोई भी अन्तर नहीं है। जिस स्रोत से आधार और अधिकार पा कर आप अपने इस शरीर में रहते और सुख भोगते हैं, उसी स्रोत से उन सब पशुओं की आत्माओं को भी जीवन का सुख भोगने का आपके समान ही अधिकार मिला है। अतः आपक किसी भी जीव की हत्या करने का नैतिक अधिकार नहीं है, भले ही वह कितना भी छोरा प्राणी क्यों न हो।
अन्तिम किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यह तथ्य है कि केवल एकमात्र वह परमचैतन ही है जिसने विभिन्न जड़ और चेतन सभी रूपों में स्वयं को प्रकट किया है। इस दृष्टि आपका समस्त सृष्टि के साथ एकत्व का सम्बन्ध है। जब आप यह जान जाते हैं, तब क्य आप किसी भी प्राणी को जानबूझ कर कष्ट या चोट पहुँचा सकते हैं? क्या आप स्वेच्छा से और प्रसन्नता से स्वयं अपनी उँगलियों को काट और पका कर खा सकते हैं? समस्त सृष्टि के साथ ऐक्य होने के इस बोध को प्राप्त करना ही, आपका इस लौकिक जगत् में बार-बार जन्म ले कर आने का कारण है। आप जब दूसरों को घायल करना, चोट या कष्ट पहुँचाना बन्द कर देते हैं और सबको अपने-आपके समान प्रेम करना प्रारम्भ कर देते हैं, केवल तभी इस एकत्व को समझ और अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में तो यह सभी पशु-पक्षी आपके अपने आत्मस्वरूप ही हैं। केवल आप ही इन सब प्राणियों में जीवात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं और आप ही इन आत्माओं के निवास हेतु देह-रूप में प्रकट हुए हैं। अतः जागें, मांस-भक्षण और पशु-हत्या करना बन्द कर दें। इनके प्रति स्नेह और परस्पर एकता की भावना को विकसित करें।
२०३
कुछ लोगों ने मुझे चेतावनी देते हुए बताया है कि प्राणायाम और शीर्षासन करना जोखिम का कार्य है और इन्हें करने से व्यक्ति पागल तक हो। सकता है। यद्यपि मुझे ऐसी बातों पर विश्वास तो नहीं है, तथापि मेरी इनके प्रति मान्यता दृढ़ भी नहीं है। कृपया मुझे बतायें कि क्या प्राणायाम और शीर्षासन के अभ्यास करने से कोई हानि होने की सम्भावना है?
आसन-प्राणायाम करते समय अपनी सीमा का अतिक्रमण न करें। अत्यधिक थक जाने तक न करते रहें। शीर्षासन और प्राणायाम करने से कोई विक्षिप्त नहीं होता। प्रत्येक कार्य करने का नियम होता है। प्रारम्भिक स्तर से आरम्भ करें और जैसे-जैसे आप अपनी उन्नति से सन्तुष्ट होते जायें, धीरे-धीरे समय की अवधि में वृद्धि करें।
२०४
एक विवाहित एवं सन्तान की माता महिला ऐसे कौन से आसन कर सकती है जो उसके लिए लाभदायक हों और जिनसे उसे कोई हानि भी न हो ?
बच्चों की माता एवं गृहणी सभी आसन कर सकती है, केवल पुरुषों की अपेक्षा उसे कुछ परिस्थितियों में कतिपय नियमों का ध्यान रखना होता है। जैसे, उसे मासिक-धर्म के दिनों में तथा उसके तीन या चार दिन बाद तक आसन नहीं करने चाहिए, किसी भी रोग से और विशेष रूप से यौन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त होने के समय तथा गर्भावस्था में भी आसन नहीं करने चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, पादहस्तासन, भुजंगासन, शलभासन और पश्चिमोत्तानासन ऐसे महत्त्वपूर्ण आसन हैं जो वह कर सकती है। इनके साथ-साथ योग मुद्रा और विपरीतकरणी मुद्रा को भी जोड़ा का सकता है। क्रिया और बन्ध तथा सूर्यनमस्कार भी किया जा सकता है। उत्तम ढंग से आसन किये जाने के लिए केवल शरीर का भारी न होना तथा शरीर में सन्तुलन होना अच्छा है, यद्यपि यह अनिवार्य शर्त नहीं है। गृहणी के लिए आसन करने में किञ्चित् भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किन्तु उसे ऊपर बताये गये नियमों का ध्यान रखना चाहिए।
२०५
'अन्तरात्मा की हत्या' का क्या अर्थ है ?
जो व्यक्ति काया, वाचा, मनसा पवित्र है, जो पाप और अधर्म करने से भयभीत होता है, जिसे भगवान् का भय है और जो पवित्र जीवन जीता है, जो समचित्त, सन्तुलित और सुस्थिरता बनाये रखने में सक्षम है, उसकी अन्तरात्मा सदैव निष्कलंकित होगी। जो व्यक्ति भरपूर सत्त्व में स्थित है, उसकी अन्तरात्मा सदैव अदूषित एवं अदग्ध होगी। हृदय की विशालता से अन्तरात्मा की आवाज़ सुनने की क्षमता में विकास होता है। उस व्यक्ति को सदैव उसकी आत्मा से निर्देश प्राप्त होते हैं जिसने जप, स्वाध्याय, प्राणायाम, निस्स्वार्थ सेवा तथा यज्ञादि जैसे उन्नत कार्यों द्वारा पर्याप्त सत्त्व अर्जित कर लिया हो।
'अन्तरात्मा की हत्या' का अर्थ है-मनुष्य के भीतर जो कुछ भी दिव्य है, उसकी हत्या कर देना, सत्त्व के वांछनीय गुण की हत्या, धर्म के सराहनीय धन की अथवा आध्यात्मिक विकास की प्रशंसनीय सम्पत्ति की हत्या कर देना। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान् का भय है, वह कभी कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उसको नैतिक विकास में अधोगति की ओर ले जाने वाला अथवा उसके नैतिक आधार को नष्ट करने वाला हो। अन्तरात्मा की हत्या करने का अर्थ मनुष्य में विद्यमान भगवान् की हत्या कर देना, समस्त दैवी सम्पत् को समाप्त कर देना और एक नृशंस एवं नरभक्षी मानव में परिवर्तित हो जाना है। अन्तरात्मा का दूसरा नाम सच्ची अथवा वास्तविक आत्मा है। इस सम्बन्ध में मेरी पुस्तक 'एथिकल टीचिंग्स' (नैतिक शिक्षाएँ) पढ़ें।
२०६
क्या सन्तान उत्पन्न करना पाप है?
न तो पुरुषत्व, न स्त्रीत्व और न ही सन्तानोत्पत्ति पाप है। सत्य अथवा परमात्म-प्राप्ति का जिज्ञासु साधक सन्तान उत्पन्न कर सकता है और बाद में संसार में रहते हुए अथवा संसार को पूर्णतया त्याग कर इस पथ पर अग्रसर हो सकता है। वशवृद्धि हेतु जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हो जाये, व्यक्ति यदि चाहे तो उसी समय सब-कुछ त्याग कर संन्यास धारण कर सकता है, यद्यपि संन्यास से पूर्व पुत्र प्राप्त होने का नियम अनिवार्य नहीं है। पुत्र की आवश्यकता, यद्यपि अत्यावश्यक नहीं तथापि यह श्रुतियों के अनुसार कहा गया है।
२०७
विवाहित पुरुष और वह भी यदि युवा हो तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है ?
शास्त्र-निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपनी पत्नी के साथ ऋतुकाल में सुख भोगना अपने-आपमें ब्रह्मचर्य का पालन है। शास्त्रों का कथन है कि विवाहित पुरुष को इन्द्रिय-सन्तुष्टि हेतु जब चाहे सम्भोग में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। उसे इन्द्रिय-सुख-भोगों तक के लिए भी निर्धारित किये गये विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए। इस विषय में विस्तृत जानकारी हेतु मेरी पुस्तक 'एडवाइज़ टू वुमैन' (महिलाओं को शिक्षा) को पढ़ें। जो व्यक्ति शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए सुखी एवं संयमित जीवन जीता है, वह गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। विवाहित दम्पति स्वभाववश कितने भी जोशीले क्यों न हों और कितने भी युवा क्यों न हों, उपर्युक्त ढंग से वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ दाम्पत्य-सम्बन्धों का पूर्ण निषेध नहीं है, अपितु इसका अर्थ भली-भाँति अनुशासित, आत्म-संयमित, धार्मिक जीवन से है।
२०८
क्या अन्तरात्मा की आवाज़ सुनने का साधन हमारी चेतना-शक्ति नहीं है?
शुद्ध चेतना ही हमारी 'आन्तरिक आवाज़' है। किन्तु सामान्य व्यक्ति की समस्या यह है कि वह अपने निम्न मन की आवाज़ को, पाशविक प्रवृत्तियों की आवाज़ को चेतना की आवाज़ समझने की भूल करता है। और ऐसी गलती के परिणाम स्वरूप पाशविक प्रवृत्तियों से प्रेरित हो कर वह ऐसी भयंकर भूलें कर बैठता है जो दूसरों को भी जोखिम में डाल देती हैं। वास्तविक अन्तरमन की आवाज़ सुनने के लिए मन की अत्यन्त उच्च स्तर की शुद्धता और प्रशान्तता की आवश्यकता होती है।
२०९
क्या मैं ये समझें कि 'शास्त्रों' से आपका आशय, शताब्दियों पूर्व लिखित अथवा अलिखित रूप में उपलब्ध प्राचीन हिन्दू धर्म द्वारा निर्धारित कठोर नियमों के ग्रन्थों से है? क्या अति शीघ्र परिवर्तित होती परिस्थितियों के कारण ये नियम एवं सिद्धान्त अब पिछड़े हुए नहीं हो गये हैं? मेरे विचार में तो कोई भी कड़ा नियम समय की परीक्षा में सफल नहीं हो सकता।
हाँ, अति प्राचीन लिखित एवं अलिखित हिन्दू धर्म के निर्धारित सिद्धान्तों के ग्रन्थों को ही शास्त्रों का नाम दिया गया है। किन्तु केवल इस कारण से इन्हें पिछड़े हुए नहीं मान लेना चाहिए। उचित जीवन जीने के मूल सिद्धान्त अपरिवर्तनशील हैं। मूल सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं होता। मूल सिद्धान्तों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो भी नही सकता।
सुधार, आंशिक बदलाव और अनुकूलन आवश्यक हैं, किन्तु बदलते हुए समय और नये वातावरण एवं नयी पीढ़ी के अनुकूल बनाने के लिए, केवल वर्णन करने की बाहा रूपरेखा और अभिव्यक्ति के ढंग में बदलाव होना चाहिए।
बाह्य परिवर्तन करने में तब तक कोई हानि नहीं है जब तक इससे मूल सिद्धान्त प्रभावित नहीं होते। मूलभूत सद्गुण यथा-सत्य, सहभागिता, अहिंसा, पवित्रता, न्याय, एकता इत्यादि मानव-जीवन पर सदैव लागू होंगे। इनका उल्लंघन सदैव भावी घोर विपनि का संकेत है।
२१०
क्या श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन भी सदैव श्रेष्ठ ही होने चाहिए? औषधि कड़वी होती है, किन्तु रोग का निवारण कर देती है। अर्जुन ने उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौरवों से युद्ध किया था।
भारतीय विचारधारा निःसंकोच इस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' में देती है। चार्वाक जैसे भौतिकवादियों के समूह को छोड़ कर शेष सभी भारतीय विचारक निर्भीक उद्घोषणा करते हैं कि, 'व्यक्ति को इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कभी भी अनुचित साधन नहीं अपनाने चाहिए, भले ही वह लक्ष्य कितना भी लुभावना क्यों न हो।' इस विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए।
मेरे विचारानुसार आपके दोनों उदाहरणों में, आपके इस कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त सुदृढ़ता नहीं है जो उद्देश्य की श्रेष्ठता में साधन के अनौचित्य को सही सिद्ध कर सके। औषधि मधुर हो अथवा कटु, यदि वह चिकित्सा के अतिरिक्त रोगी को अथवा अन्य किसी को भी कोई हानि नहीं पहुँचाती, तो वह साधन के रूप में दोष रहित है। यह उद्देश्य-प्राप्ति अर्थात् रोग-निवारण के लिए अपनाया गया उचित साधन है।
दूसरे उदाहरण में, निःसन्देह अर्जुन ने कौरवों के साथ युद्ध किया था, और उन सबका बध भी किया था; किन्तु अर्जुन द्वारा किया गया युद्ध उसकी क्रूरता को प्रदर्शित नहीं करता, अपितु उसके कर्तव्य-पालन को दर्शाता है। युद्ध तो उसके भाग्य पर थोप दिया गया था जिसे करना अब उसका कर्तव्य अथवा उसका स्वधर्म हो गया था, अर्जुन ने स्वयं युद्ध की कामना नहीं की थी। उसने कौरवों को युद्ध करने के लिए बाध्य नहीं किया था, अपितु उन्होंने इसे चुनौती दी थी। उसने अपनी और अपने परिजनों की रक्षा तो करनी ही थी। अपने अधिकारों की रक्षा हेतु युद्ध करना उसका पावन कर्तव्य एवं नैतिक दायित्व था। अतः अर्जुन का युद्ध करना, उसकी कर्तव्य-बद्धता के कारण पूर्णतया न्यायसंगत है।
भगवान् श्री कृष्ण ने भगवद्गीता में अनेक स्थानों पर बारम्बार इस बात को दोहराया है। इसके विपरीत यदि अर्जुन युद्ध करने के अपने कर्तव्य से पलायन कर जाता तो वह अपने धर्म का निर्वाह करने से चूक जाता। अतः भगवान् पुनपुनः उसे निर्देश देते हैं, 'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि' (अपने समक्ष आये हुए इस धर्म को देख कर इससे पीछे मत हटो), 'युद्धस्व विगतज्वर' (मन के संशय को त्याग कर युद्ध करो), इत्यादि।
२११
जब मृत्यु पूर्व-निश्चित है और वस्त्र परिवर्तन कर लेने के लिए एक विराम-काल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो फिर आत्महत्या करना और किसी कारण से अन्य प्राणियों की हत्या करना भी पाप क्यों है ?
आत्महत्या और दूसरों की हत्या करना-दोनों ही पाप माने जाते हैं, क्योंकि वह जीव-विकास-क्रम को अवरुद्ध करते हैं। इससे भी बढ़ कर यह कि वर्तमान देह को बलात् समाप्त कर देने से व्यक्ति के कष्टों की समाप्ति नहीं हो जाती। गत जन्मों में किये गये कर्मों के परिणामस्वरूप इस जन्म में मिलने वाले सुखों अथवा दुःखों को पूर्णतया भोग लेने से ही उन कर्मफलों से छुटकारा मिलता है।
इसके विपरीत, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए और भी अधिक कष्टों को आमन्त्रित कर लेता है, क्योंकि शेष कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः नया शरीर मिलने में समय लगेगा और इस अन्तरिम काल में उसको प्रेत हो कर रहना पड़ सकता है। और निश्चित रूप से यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि अन्य किसी भी मनुष्य की हत्या करना तो न्यायिक दृष्टि से अपराध है ही, आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी अत्यन्त घृणित पाप है। हाँ, युद्धभूमि जैसी परिस्थिति में ऐसा नहीं है।
२१२
हमारे पूर्वजों की अपेक्षा आधुनिक काल के मानव की आयु इतनी अल्प क्यों है ?
हमारे पूर्वज एक नियमित एवं अनुशासित जीवन जीते थे। आधुनिक मानव की भाँति वे इन्द्रियों के दास नहीं थे। वे जप, प्राणायाम, त्रिकाल-सन्ध्या-वन्दन तथा गीता, भागवत और रामायण जैसे धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय किया करते थे। वे दान, निष्काम सेवा तथा श्री रामनवमी, श्री कृष्णजन्माष्टमी और दत्तात्रेय जयन्ती जैसे दिनों में उपवास करते थे। वे आध्यात्मिक सम्मेलनों का आयोजन करते थे तथा अपने लिए नहीं अपितु विश्व-शान्ति के लिए प्रार्थनाएँ किया करते थे। वे प्रतिदिन एक-साथ १० से २० मील तक की सैर करने जैसा व्यायाम करते थे। यम और नियमों का वे अत्यन्त कठोरता से पालन करते थे। वे भीड़-भरे नगरों में न रह कर गाँवों में रहते थे। वे छोटे-छोटे कामों के लिए भी किसी पर आश्रित नहीं रहते थे और अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करते थे। उन्हें काया-सिद्धि और वाक्-सिद्धि दोनों ही प्राप्त थीं। जब आधुनिक पीढ़ी के लोग प्राचीन जीवन-पद्धति का मूल्य समझेंगे, तब निश्चित रूप से देवों की प्रसन्नता प्राप्ति से समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगी।
२१३
आपके विचारानुसार एक आध्यात्मिक रुचि-सम्पन्न गृहस्थ के कितनी सन्तान होनी चाहिए ?
प्रत्येक गृहस्थ, भले ही आध्यात्मिक विचारों का हो अथवा सांसारिक विचारों वाला हो, वंश को चलता रखने के लिए पुत्र की कामना रखता है और वह देवी माँ प्रकृति, जिनसे समस्त संसार की उत्पत्ति होती है, देवी माँ प्रकृति जो सृष्टि की रचयिता एवं आधार हैं, उनके अकथनीय प्रकाश की अभिव्यक्ति हेतु वह एक पुत्री की कामना भी रखता है। कोई भी गृहस्थ केवल पुत्र अथवा केवल पुत्री ही होने से सन्तुष्ट नहीं होता। पुरुष और प्रकृति के प्रतिनिधि वे दोनों ही अपनी अपनी निजी अभिव्यक्ति के रूप में दोनों सन्तानों की इच्छा रखते हैं। पुत्र और पुत्री के अतिरिक्त मृत्यु इत्यादि जैसी दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं को देखते हुए एक सन्तान और की जा सकती है। आध्यात्मिक रुचि सम्पन्न गृहस्थ तीन सन्तानों के जन्म होने तक वैवाहिक जीवन जी सकता है। इसके उपरान्त शीघ्र उन्नति के लिए एवं साक्षात्कार प्राप्ति के लिए वह निवृत्ति-मार्ग अपना सकता है। तुकाराम, रामतीर्थ और पोथना जैसे सन्तों के जीवन-चरित्र पढ़ें। तब आपको 'संसार में रह कर और संसार के माध्यम से साक्षात्कार' कथन में निहित सत्य का बोध होगा। कामासक्ति के आधिक्य के अथवा अति सांसारिकतापूर्ण जीवन की आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुँच नहीं हो सकती। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना भी आवश्यक है कि साक्षात्कार अथवा मोक्ष के लिए सन्तानोत्पत्ति अनिवार्य नहीं है कि जिनके सन्तान नहीं है, वे मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं और साथ ही यह भी कि जो वंश-वृक्ष की वृद्धि न करके संन्यास ग्रहण करेंगे, वह देवताओं के प्रकोप से मुक्त रहेंगे।
२१४
स्वामी जी, आप अपने पैरों की पूजा क्यों करने देते हैं, क्यों नियमित रूप से उनकी पूजा करने की आज्ञा दे देते हैं?
आधुनिक भौतिकता से ग्रस्त मन के लिए इसे समझने से पहले भलीभाँति शुद्धिकरण की आवश्यकता है। आध्यात्मिक साधक के लिए गुरु के पाँव केवल पाँव मात्र नहीं, अपितु वे दिव्य कृपा के वाहक हैं। स्मरणातीत काल से ही भारतीय जिज्ञासु साधक यह जानता और मानता है कि उसका संग्राहक-केन्द्र (रिसैप्टिव सेंटर) अर्थात् शिर, उसके गुरु के प्रेषक-केन्द्र (ट्रांसमिटिंग सैंटर), उनके चरणों के सम्पर्क में आना चाहिए, जिससे कि उसमें आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और प्रकाश अनुप्राणित हो सके। विद्युत् के सिद्धान्तों में से एक यह स्वतः सिद्ध तथ्य है कि विद्युत् का एक परिपथ पूर्ण करने के लिए ऋणात्मक (नैगेटिव) और धनात्मक (पौज़िटिव) बिन्दुओं का परस्पर सम्पर्क होना अनिवार्य है।
पादपूजा करने से साधक के मन में आत्मसमर्पण का भाव जागृत होता है। फूल हृदय का प्रतीक हैं, फल कर्मफलों का प्रतीक, सिक्के समस्त सम्पत्ति के और कर्पूर साधक की उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जो गुरु की प्रबुद्ध आत्मा में पूर्णतया लीन हो चुकी है। इन सभी प्रतीकात्मक पदार्थों को सर्वप्रथम पूजा में समर्पित किया जाता है। फिर अन्त में शिष्य अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, जो इस बात का प्रतीक है कि किञ्चित् भी शंका अथवा संकोच के बिना वह अपना सर्वस्व सद्गुरु को समर्पित कर रहा है।
पादपूजा साधक शिष्य में श्रद्धा और भक्ति की भावना को सुदृढ़ करते हुए उसमें विनम्रता इत्यादि दैवी गुणों को विकसित करती है।
भरत ने भगवान् श्रीराम के दिव्य चरणों की पूजा की थी और उन्होंने उनकी पादुकाओं को ले जा कर श्रीराम के प्रतिनिधि के रूप में सिंहासनारूढ़ किया तथा स्व को पादुकाओं का संरक्षक मानते हुए राज्य की सेवा की। ऐसी विनम्रता, श्रद्धा आ विश्वास आपको भी दिव्य बना देंगे।
यहाँ मैं लोगों को आने और पादपूजा करने के लिए विवश नहीं करता हूँ, यदि वे ऐसा करते हैं तो अपनी इच्छा से करते हैं, और मेरे प्रति अपनी गुरुभक्ति के कारण ऐसा करने का आग्रह करते हैं तो मैं अस्वीकार नहीं कर पाता। यदि मैं अस्वीकार कर दूँ तो न केवल उन्हें निराश करूँगा जो मुझे सम्मानपूर्वक आत्मसमर्पण करने को आतुर हैं, अपितु स्वयं अपने कर्तव्य से भी विमुख हो जाऊँगा। आप क्या यह सोचते हैं कि मैं अपनी पादपूजा करने से प्रसन्न और सम्मानित होता हूँ? इस सारी प्रक्रिया में मुझे धैर्य सहित चुपचाप बैठे रहना पड़ता है और यह निश्चय ही, अपनी प्रसन्नता के लिए धैर्यपूर्वक बैठे रहने को नहीं मान जाता हूँ!!
२१५
एक विवेकशील व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में मूलतः क्या चिह्न दृष्टिगोचर होता है ?
मूर्ख मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में भावनाओं के वश में हो कर बाह्य रूप से तत्काल प्रतिक्रिया कर देता है जब कि साधु स्वभाव वाले व्यक्ति में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। यदि वह कुछ करता भी है तो वह उसी समय किये गये किसी भी कार्य अथवा व्यवहार की प्रतिक्रियावश नहीं अपितु उस सन्त के मानवता के प्रति सेवाभाव से उत्पन्न सत्संकल्पवश होता है। दूसरा लक्षण यह है कि मूर्ख मनुष्य परिस्थिति में स्वयं को सबसे प्रथम स्थान देता है; किन्तु अन्ततः अपने-आपको अन्तिम स्थान पर पाता है, जब कि विवेकी व्यक्ति अपने-आपको सबसे पीछे रखते हुए भी सर्वप्रथम स्थान पर पाता है। तीसरा बुद्धिमान् व्यक्ति कार्य पूरा करने के उपरान्त चुपचाप पीछे हट जाता है, किन्तु पूर्व अन्य लोगों से, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वहीं बैठा रहता है और कोई-कोई तो यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो वह निर्लज्जता सहित प्रशंसा करने के लिए कह तक देता है।
कृपया भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय को भी पढ़ें जिसमें आपको स्थितप्रज्ञ का विवरण प्राप्त हो जायेगा।
२१६
मनुष्य में अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली क्या है-क्षुधा अथवा कामेच्छा ?
जीवमय इस जगत् में समस्त प्राणी-वर्ग में तीन वस्तुएँ समान हैं-आहार, निद्रा और मैथुन। मनुष्य में आहार की भूमिका इतनी अधिक महत्त्व नहीं रखती जितनी कामेच्छा की। यह पुरुषों में १६ वर्ष की तथा स्त्रियों में १४ वर्ष की किशोरावस्था में विकसित हो जाती है। यह आयु सीमा न्यूनतन मात्र है और ऋतुओं, वातावरण तथा व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार अधिक या कम हो सकती है। स्त्री अथवा पुरुष ने भले ही अभी युवावस्था में पूरी तरह प्रवेश किया भी न हो, उसमें कामेच्छा स्वाभाविक रूप में गतजन्मों के संस्कारों के प्रभाव से तथा बाह्य जगत् के सामान्य दृश्यों को देखने के कारण विद्यमान रहती है। किसी व्यक्ति ने भले ही कई दिनों से आहार ग्रहण न भी किया हो यौनेच्छा अथवा कामेच्छा तो भी उसमें रहेगी ही। यहाँ तक कि जब आयु-आधिक्य अथवा किन्हीं अन्य कारणों से कामेच्छा क्षीण पड़ जाती है या समाप्त भी हो जाती है तो भी उसकी वासना अथवा कामपूर्ति की कल्पना, काम-सुख-भोग के स्वप्न लेने की चाह नहीं मिटती, अपितु मन के किसी अज्ञात कोनों में दबी रहती है जो किसी भी सुन्दर एवं सुखद घटना या दृश्य को देखने या पढ़ने से मनुष्य पर हावी हो जाती है और उसके मन को अतीत के किसी भी अनुभव की स्मृतियों में पहुँचा देती है। यह सब स्पष्टतया सिद्ध करता है कि कामाग्नि, क्षुधाग्नि से अधिक प्रबल या शक्तिशाली है। जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने से अग्नि और अधिक प्रचण्ड हो जाती है, उसी प्रकार कामेच्छा की शारीरिक पूर्ति से वह और भी अधिक प्रबल होती है। क्षुधापूर्ति कर लेने से वह शान्त हो जाती है, किन्तु कामेच्छा की भूमिका मनुष्य के जीवन में मुख्य स्थान पर रहती है।
२१७
यदि किसी व्यक्ति का बलपूर्वक ऐसी लड़की से विवाह कर दिया गया हो जो सुन्दर तो बिलकुल भी न हो किन्तु उसमें सद्गुण शिर से पाँवों तक भरपूर हों, तब उस पुरुष को अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए जब कि अपनी पत्नी की कुरूपता की चिन्ता उसके मन को निरन्तर कचोटती रहती हो ? पत्नी में सुन्दरता के अभाव से उत्पन्न भीतर इकट्ठी हुई कुण्ठा की भावनाओं को वह कैसे नियन्त्रित करे, कैसे उन्हें अच्छी तरह से छुपाये और फिर स्वस्थ, सुखद एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करे ?
यह पुरुष के हाथ में नहीं है कि वह इस या उस सुन्दर लड़की को अपने साथ विवाह के लिए चयन करे, न ही किसी लड़की के वश में है कि वह अमुक सौन्दर्यवान् अथवा धनाढ्य पुरुष का अपने लिये चयन करे। सब-कुछ पूर्व-निर्धारित है। मनुष्य इस स्पष्ट दिखायी देने वाले तथ्य को भुला देता है, इस महत्त्वपूर्ण सत्य की उपेक्षा कर देता है तथा यह सोचता और समझता है कि वही वास्तव में कर्ता एवं भोक्ता है। स्वयं से यह कहें और अपने-आपको सान्त्वना दें, 'दैवाधीन, दैवाधीन। भगवान् की इच्छा, परमात्मा की इच्छा।' मन में ऐसा विचार करें और यह मान कर चलें कि आपके जीवन में आपके साथ हर क्षण जो कुछ भी हो रहा है, उसमें ही आपका सर्वोत्तम भला है। इस महान् सत्य में दृढ़ विश्वास रखें और दार्शनिक उदासीनता एवं वैराग्यपूर्ण उदासीनता में आनन्दित रहें। शारीरिक सौन्दर्य किश्चित् भी वास्तविक सौन्दर्य नहीं। यह तो केवल ऊपरी त्वचा में ही रह जाता है। जिस नारी के पास पवित्रता के सद्गुणों का सौन्दर्य है, वही वस्तुतः विश्व में सर्वाधिक सुन्दर नारी है। यह हमारे महान् नीतिदाता मनु महाराज की उद्घोषणा के अनुरूप है। मनु के नीतिशास्त्र, मनुस्मृति का अध्ययन करें। मनु के इस कथन को मन में बार-बार दोहरायें, 'पवित्रता सौन्दर्यहीन नारी का सौन्दर्य है।'
सुन्दरता और कुरूपता केवल मन की कल्पनाएँ हैं, जैसे मिठास और कड़वाहट मन में और केवल मन में ही निहित हैं। इस मन के धर्म ही ऐसे हैं। मन से ऊपर उठें। तब आप कुरूपता में सौन्दर्य, कड़वे में मिठास और बुराई में भलाई को देख सकेंगे। विकास की उच्चावस्था पर पहुँच जाने पर भलाई, मिठास और सुन्दरता के विचार तक ही समाप्त हो जाते हैं।
हाथ सेवा के लिए हैं, हृदय प्रेम एवं भक्ति के लिए और शिर बुद्धि एवं ज्ञान के लिए है। यह अत्यन्त विलक्षण सम्मिश्रण है, जो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। नारी की वास्तविक सुन्दरता उसके मन के भीतर की वह पवित्रता है, जो प्रथम दृष्टि में ही मनुष्य को परम सुख से रोमाञ्चित कर देती है और उसे परम आनन्द की उँचाइयों तक पहुँचा देती है। इसे ही वास्तविक सौन्दर्य कहा जाता है।
कोई भी वस्तु अपने नकारात्मक गुणों के कारण भले ही कितनी भी निन्दनीय क्यों न हो, सदैव उसमें भला, सुन्दर, शुभ और सुखद देखने का प्रयत्न करें। तब और केवल तब ही आप परमात्मा तक की असीम उँचाइयों तक उन्नत तथा प्रचुर मात्रा में विकसित हो सकेंगे। जब तक व्यक्ति स्वयं को सीमित धारणाओं में बद्ध रखता है और मन में संशयपूर्ण, नकारात्मक एवं द्वैत की भावनाओं को पालता रहता है तब तक उसे विकसित जीव नहीं माना जा सकता। भारतवर्ष के सग्रन्थों की साकार प्रतिमा जैसी जो आदर्श पतिव्रता के सद्गुणों से सम्पन्न महिला है, उसके सम्मुख मानसिक प्रणिपात करें। स्वयं को सुधारें। इस बात को अनुभव करें कि आपका पद, आपकी उपाधि, आपकी वित्तीय सामर्थ्य और आपका व्यक्तित्व, इन सबकी यदि आपकी पत्नी के सद्गुणों की सम्पदा से तुलना की जाये तो वह सब केवल तुच्छ कचरे के समान है। जीवन का अहंकारपूर्ण अनुमान करने की भावना का परित्याग कर दें।
२१८
क्या सिनेमा देखना हानिकारक है? क्या इससे लोगों का चरित्र दूषित हो जाता है? कृपया यह बताने का अनुग्रह करें।
सिनेमा अपने-आपमें हानिकारक नहीं है, किन्तु बिना सोचे-समझे अत्यधिक सिनेमा देखने से सामान्यतया लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और दृष्टि मन्द हो जाती है। साथ ही इससे बहुत सी कुसंगति मिलने की भी सम्भावना बनी रहती है। यह सबसे अधिक दोषपूर्ण तब हो जाता है, जब यह ऐसे कामुक दृश्यों से भरा होता है जो काम-वासनाओं की वृद्धि करने वाले, इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाले और वासनाओं, घृणा, झूठे अभिमान, उद्वेग अथवा किसी भी प्रकार की विषयासक्ति या अहंकार को उत्पन्न करने का कारण हों। हाँ, निस्सन्देह शिक्षाप्रद, धार्मिक और आध्यात्मिक चलचित्र देखने में कोई हानि नहीं है, यद्यपि मनुष्य में सदा ही नैतिक नियमों और सुसंस्कृत स्वभावानुकूल निर्धारित की गयी सीमाओं का अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति पायी जाती है।
२१९
समस्त संशयों और प्रश्नों का स्थायी अन्त कैसे किया जा सकता है?
समग्र योग के नियमित एवं सतत अभ्यास के द्वारा व्यक्ति जैसे-जैसे आध्यात्मिक साधना में उन्नत होता हुआ दिन-प्रति-दिन विकास के उच्च से उच्चतर आयाम को प्राप्त करता जाता है, वैसे-वैसे ही उसके संशयों, भ्रान्तियों और प्रश्नों के बादल स्वयं ही छँटने लगते हैं। जैसे सूर्य के उदित होते ही कोहरा छँट जाता है, उसी प्रकार जैसे-जैसे आप आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करते हैं, गुरु एवं भगवान् की कृपा से जीवन-मरण की सभी गहन समस्याएँ सच्चिदानन्द भगवान् में स्वयं ही लीन हो जाती हैं। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य विकसित समग्र साधना द्वारा आन्तरिक पवित्रता को बढ़ाते जाना है। जब भी कोई संशय, समस्या या कठिनाई उत्पन्न हो, तो नीचे लिखे मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र का जप करें: 'ॐ श्री राम शरणं मम', 'ॐ श्री कृष्ण शरणं प्रपद्ये' अथवा अपना गुरु-मन्त्र। ईश्वर-साक्षात्कार के उपरान्त संशय उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि तब साधक एक साधक न रह कर स्वयं परमात्मा हो जाता है।
२२०
मैं कभी-कभी भगवान् की महिमा और उनकी सर्वव्यापकता पर ध्यान किया करता हूँ, किन्तु उससे मुझे कुछ अधिक लाभ मिलता प्रतीत नहीं होता। इसका क्या कारण है, क्या आप बताने की कृपा करेंगे?
भगवान् का ध्यान कभी-कभार करने का कोई लाभ नहीं है। जप और ध्यान प्रति दिन, बिना एक भी दिन छोड़े, निर्बाध करें। जैसे आप चाय और भोजन प्रतिदिन करते हैं और जैसे आप उन्हें करना भूलते भी नहीं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में साधना करना न छोड़ें, भूल से भी नहीं। सर्वप्रथम अपनी साधना करें। थोड़ी-बहुत, जितनी भी आप कर सकते हैं, उतनी करें- केवल तभी अपना भोजन ग्रहण करें। मन को निर्बाध और गम्भीरता सहित साधना में प्रवृत्त करने का यह सुनिश्चित, सशक्त और सफल ढंग है। यह पद्धति अपनाने से आपका नियमित रूप से साधना करने का स्वभाव बन जायेगा, भले ही साधना करने को मन न भी चाह रहा हो कम-से-कम उसके उपरान्त मिलने वाले भोजन के लिए ही सही।
जब मन को बीच-बीच में सांसारिक सुख लेने का समय मिलता रहता है, तो यह स्वयं पर केन्द्रित होने और अपने भीतर उतरने में सक्षम नहीं हो पाता। जब मन इधर-उधर भागता है तो इसकी लगाम को अपने भीतर की ओर खींचें। यह प्रक्रिया दिन में बार-बार दोहरायें। जब कठोर अभ्यास के माध्यम से भगवान् का अपने भीतर साक्षात्कार करने की शक्ति विकसित कर लेते हैं, तो उन्नति स्वयमेव होने लगती है। गीता के द्वितीय अध्याय का अर्थ सहित स्वाध्याय करें। इससे आपको साधना की प्रगति में बाधाओं के सम्बन्ध में स्पष्टतया बोध हो जायेगा।
२२१
यदि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता की पावन इच्छाओं की उपेक्षा करके साधु बन जाता है, तो क्या यह अवज्ञा करने का पाप नहीं है?
निःसन्देह यदि व्यक्ति अपने माता-पिता, निकट सम्बन्धियों अथवा प्रियजनों से आज्ञा ले कर साधु या संन्यासी बनता है तो यह उस व्यक्ति के लिए अच्छा है। किन्तु यदि उच्च श्रेणी का वैराग्य हो जाने पर वह निवृत्ति मार्ग को अपनाना चाहता है तो ऐसा करने में बिलकुल भी हानि नहीं है।
वस्तुतः इस संसार में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी भी मनुष्य का किसी से कोई नाता नहीं है और एक-दूसरे का परस्पर जो भी नाता है, वह केवल गत जन्मों के कर्मों के कारण ही है। बहती नदी में दो लकड़ी के शहतीरों की भाँति मनुष्यों का परस्पर संयोग और वियोग होता है। जब समय हो जाता है तो सब-कुछ उस एक में विलीन हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति को तीव्र वैराग्य हो जाये और जब उसमें यह सुदृढ़ भावना उदित हो जाये कि इस संसार में कोई किसी का नातेदार नहीं है और प्रत्येक ने अपना परम लक्ष्य स्वयं प्राप्त करना है तो वह अपने इच्छित समय पर संन्यास ग्रहण करने के लिए स्वतन्त्र है।
२२२
क्या आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि स्वर्ग और नरक का इस भू-लोक से अलग कहीं अन्यत्र स्वतन्त्र अस्तित्व है ?
क्यों नहीं? हमारे इस भू-लोक की भाँति अन्य लोक भी हैं। उनका अस्तित्व भी उतना ही वास्तविक है जितना हमारे इस लोक का। यदि व्यक्ति अपने शास्त्रों में विश्वास रखता है तो समस्त लोक और सभी तीर्थ मनुष्य के अपने शरीर में ही विद्यमान हैं। यदि मनुष्य चाहे तो वह इस जन्म में ही नरक या स्वर्ग भोग सकता है। व्यक्ति में जितनी अधिक मलिनता होगी, उसे उतने ही अधिक कष्ट, यातनाएँ और उत्पीड़न, उस समय तक रहेंगे जब तक वह बार-बार भस्मीकरण प्रक्रिया अथवा शुद्धिकरण प्रक्रिया द्वारा स्वयं को भगवान् के अवतरण के योग्य नहीं बना लेता। यदि आप इस धरती पर ही स्वर्ग के भोग भोगने के इच्छुक हैं, तो अपने निम्न मन, इच्छाओं और लालसाओं को नियन्त्रित करके स्वयं को शुद्ध करते जायें। तब सर्वत्र आनन्द है, सर्वदा सुख है, सब ओर प्रसन्नता है। यदि आप इन्द्रियों के अश्वों की लगाम खुली छोड़ देते हैं और आसुरी मन की उत्तेजक कामनाओं के समक्ष घुटने टेक देते हैं, यदि आप अधर्म के पथ को स्वीकृति दे देते हैं, तो नरक यहीं उपस्थित हो जायेगा, कहीं दूसरे लोक में नहीं, यहाँ इसी भू-लोक में, आपके अपने निकट !
२२३
मुस्लिमों के लिए कुरान है, ईसाइयों की बाइबल, यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट, पारसियों की गाथाएँ हैं। हिन्दुओं के लिए क्या है ?
निःसन्देह गीता। यह समस्त हिन्दुओं के लिए सरल और आधारभूत ग्रन्थ है। इसमें उपनिषदों का सार निहित है, यह जीवन का सकारात्मक एवं आदर्श दर्शन प्रदान करती है और योग के समन्वयात्मक प्रमुख पथ दर्शाती है।
२२४
आप तो समानता के पक्षपाती हैं और आप अपनी शिक्षाओं में जाति-पाति का भेद-भाव नहीं मानते तो क्या आप साम्यवाद के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं?
मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है और किसी भी अनीश्वरवादी मत से तो प्रश्न ही नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता कि धर्म अथवा धार्मिक शिक्षाओं का राजनीति से कोई सम्बन्ध होना चाहिए। समदृष्टि से मेरा अभिप्राय यह है कि समस्त प्राणियों में वह एक हो परम सत्ता समान रूप में विद्यमान है। नाम और रूप परिवर्तनशील हैं। केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। सापेक्ष दृष्टि से समस्त मानवता भगवान् का एक परिवार है, भगवान् की दृष्टि में कोई उच्च या नीच नहीं है। अतः आध्यात्मिक व्यक्ति का व्यवहार जाति, धर्म, वर्ण, मत-मतान्तर अथवा पद-प्रतिष्ठा के भेदभाव के प्रभाव से किसी भी प्रकार से संकुचित नहीं होना चाहिए।
२२५
भगवान् चेतन हैं अथवा जड़ ? यदि वह चेतन हैं तो निश्चित रूप से उनका कोई रूप भी होना चाहिए, क्योंकि चेतना तो केवल उसी में हो सकती है जिसका कोई रूप-आकार हो।
भगवान् शुद्ध चैतन्य हैं। वह सर्वज्ञ हैं, सब-कुछ जानते हैं। वह निराकार अथवा अमूर्त हैं। इस भौतिक शरीर ने हमारी परम चेतना को सीमाबद्ध कर दिया है। चेतना विभिन्न प्रकार की होती है, यथा-भौतिक अथवा शारीरिक चेतना, मानसिक चेतना और परम चेतना। परमचैतन्य की अनुभूति आपको तब होगी जब सतत एवं गहन ध्यान के द्वारा आप तीनों शरीरों से अतीत पहुँच जायेंगे। इस सीमित देह और सीमित इन्द्रियों से तो आप केवल भौतिक अथवा शारीरिक चेतना को ही अनुभव कर सकते हैं।
२२६
यदि मैं कहता रहूँ कि 'मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ' तो मैं राजा नहीं बन सकता, इसी प्रकार यदि मैं 'अहं ब्रह्मास्मि' का जप करता रहूँ तो मैं ब्रह्म नहीं बन सकता।
'मैं राजा हूँ' कहने के साथ-साथ आपको स्वयं को तैयार भी करना पड़ेगा। आपको भारी संख्या में लोग एकत्रित करने होंगे। और भी बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। युद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए भी इसी प्रकार आपको तैयारी करनी होगी और मन को शुद्ध करना होगा। मोक्ष प्राप्ति के चारों साधनों, यथा- विवेक (नित्य-अनित्य के भेद को समझने का ज्ञान), वैराग्य (आसक्ति का न होना), षड्सम्पद (षड्गुणों का अर्जन) और मुमुक्षुत्व (मुक्त होने की तीव्र आकांक्षा) को अर्जित करना होगा। इसके उपरान्त श्रवण (श्रुतियों को सुनना), मनन (सुने-पढ़े हुए पर गहन विचार) और निदिध्यासन (सतत एवं गहन ध्यान) करना पड़ेगा। केवल तब ही आप आत्म-साक्षात्कार अथवा ब्रह्मानुभूति प्राप्त कर सकते हैं।
२२७
यदि मैं 'शर्करा, शर्करा' कहता रहूँ तो मुझे शर्करा प्राप्त नहीं हो सकती। तब क्या यदि मैं 'राम, राम' कहता रहूँ तो क्या राम प्राप्त हो सकते हैं?
शर्करा क्रय करने के लिए पहले तो आपको धन चाहिए, फिर लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। इसी प्रकार इसके लिए भी आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, मद एवं मात्सर्य का त्याग करना होगा; फिर भाव एवं निष्ठापूर्वक एकाग्रता के साथ 'राम, राम' जप करना होगा। तब आपको भगवान् श्री राम के दर्शन अवश्य प्राप्त से जायेंगे। किन्तु राम तो आपके भीतर हैं। शर्करा बाहर है। आपको अपना हृदय पूर्ण रूप से श्री राम को समर्पित करना पड़ेगा।
२२८
समाधि में अति शीघ्र कैसे प्रवेश किया जा सकता है?
यदि आप अति शीघ्र समाधि में प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने मित्रों, सम्बन्धियों आदि के साथ समस्त सम्बन्धों का विच्छेद कर डालें। किसी को भी पत्र न लिखें। एक मास के लिए पूर्ण मौन धारण कर लें। एकान्त में निवास करें। अकेले भ्रमण करें। अत्यन्त अल्प किन्तु पुष्टिवर्धक आहार लें, यदि रह सकते हों तो केवल दूध पी कर निर्वाह करें। गहन समाधि में उतर जायें। और भी अधिक गहन गोता लगायें। निरन्तर अभ्यास करते रहें। आप समाधि में लीन हो जायेंगे। अपनी सामान्य बुद्धि का उपयोग करें। मन के साथ बल-प्रयोग न करें। शान्त रहें। दिव्य विचार तरंगों को शान्तिपूर्वक प्रवाहित होने दें।
२२९
बुराई के होने की आवश्यकता ही क्या है?
यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका अभी तक सन्तों, ऋषियों, आचायों और दार्शनिकों ने भी उत्तर नहीं दिया है। आप अभी यह प्रश्न न करें। अपने विकास के जिस स्तर पर अभी आप हैं, उस पर अभी आप इसे नहीं समझ पायेंगे। यह अवर्णनीय है, अबोधगम्य है, अनिर्वचनीय माया है। केवल ब्रह्म अथवा भगवान् ही इसे जानते हैं। आप इसे केवल तभी समझ सकेंगे जब माया से मुक्ति पा लेंगे, जब आपको ब्रह्म का बोध अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जायेगा। यह प्रश्न एक अन्य ढंग से भी किया जाता रहा है। भगवान् ने इस सृष्टि की क्यों रचना की? इस विश्व के, क्यों और कैसे के सम्बन्ध में कोई नहीं जानता। आप भी अब इस विषय पर माथापच्ची न करें। अभी आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, केवल अपना समय और शक्ति ही नष्ट करेंगे। आप अभी केवल बुराई से परे जाने का प्रयास करें। इसके मार्ग हैं, उन्हें जानें और प्रयत्न करें।
२३०
इच्छाओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है?
विवेक-शक्ति को विकसित करें। ब्रह्म सत्य है। जगत् मिथ्या है। ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मन में है। विचार करें। समस्त इच्छाएँ शून्य में लीन हो जायेंगी। वस्तु-पदार्थों में दोष-दृष्टि से विचार करें। विषय-वस्तुएँ असत् हैं, जड़ हैं एवं दुःख का कारण और अशुद्ध हैं। ज्वलन्त मुमुक्षुत्व को विकसित करें। आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अन्य समस्त सांसारिक इच्छाओं को नष्ट कर देगी। अपनी इन्द्रियों को भी नियन्त्रण में रखें। वैराग्य को बढ़ायें। भोग-पदार्थों को छोड़ दें। यह त्याग है। इससे समस्त इच्छाएँ समाप्त हो जायेंगी।
२३१
यदि हम भगवान् के हाथों का उपकरण मात्र हैं, तो क्या मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है?
मनुष्य केवल तभी स्वतन्त्र होता है जब उसकी व्यक्तिगत इच्छा भगवान् की इच्छा में लीन हो जाती है। स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता को आध्यात्मिक स्वतन्त्रता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान् के हाथों का निमित्त अथवा उपकरण बनने से भक्त अपने अहंकार अथवा अपनी 'तुच्छ मैं' को नष्ट कर देता है, किन्तु उसे समस्त दिव्य ऐश्वर्य अथवा भगवान् की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। अब वह भगवान् के साथ एक हो गया होता है।
२३२
मैं स्वयं को ध्यानपरायण जीवन जीने के लिए किस प्रकार तैयार करूँ ?
अपनी धन-सम्पत्ति अपने तीनों पुत्रों में बाँट दें। जीवन-निर्वाह के लिए थोड़ा-सा अपने पास रख लें। कुछ अंश दान कर दें। ऋषिकेश में एक कुटीर बना लें और वहाँ रहें। अपने पुत्रों को पत्र न लिखें। मैदानी क्षेत्र में न जायें। इसके उपरान्त ध्यान आरम्भ करें। अब आपका मन शान्त हो जायेगा। यह सब-कुछ तत्काल आरम्भ कर दें। शीघ्रता करना अति आवश्यक है।
२३३
जब मैं उत्तरकाशी में रह रहा था तो मैं उत्तम निष्ठा, उदात्त वृत्तियों तथा श्रेष्ठ धर्म की भावना से सम्पन्न था। अब यहाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते ही वह सब लुप्त हो गयी हैं, यद्यपि साधना मैं अब भी करता हूँ। ऐसा क्यों ? पहले की भाँति स्वयं को मैं कैसे उन्नत करूँ ?
सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों का सम्पर्क तत्काल मन को प्रभावित कर देता है। विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। मन अनुकरण करता है। कुप्रवृत्तियाँ और विलासप्रियता बढ़ने लगती है। अनुपयुक्त वातावरण और कुसंगति अत्यन्त गहरा प्रभाव डालते हैं जो साधक के मन को आच्छादित कर देते हैं। पुराने संस्कार पुनः हावी होने लगते हैं। मैं आपको पुनः तुरन्त उत्तरकाशी लौट जाने का परामर्श दूँगा। एक क्षण का भी विलम्ब न करें। भोजन के सूक्ष्म अंश से मन की रचना होती है, अतः यह भोजन बनाने वाले के साथ आसक्त हो जाता है। किसी के भी आभार के तले न आयें। स्वतन्त्र जीवन यापन करें। स्वयं अपने-आपके ऊपर निर्भर रहें।
२३४
भगवान् क्या हैं?
यदि मैं आपके एक अच्छा सा ज़ोरदार थप्पड़ लगा दूँ, तो उस थप्पड़ को कौन जानता है? वह जानने वाला 'वेत्ता' भगवान् हैं। जब किसी तीव्र इच्छा की पूर्ति होती है, तब आनन्द की वह अवस्था जिसमें मन शान्त हो जाता है, वह भगवान् हैं। आपके नेत्रों को प्रकाशित करने वाली ज्योति भगवान् हैं। आपके चिन्तन की स्फुरणा भगवान् हैं, वहीं आपके मन के रचयिता हैं, आपके मन के स्रोत, उसका आधार, आपके प्राण, इन्द्रियों और शरीर के अधिष्ठान भगवान् हैं।
वृक्ष का अस्तित्व है, यह प्रफुल्लित है, उद्भासित है, यह प्रसन्नता देता है। यह तीन पक्ष-अस्ति-भाति-प्रिय अथवा सत्-चित्-आनन्द-भगवान् हैं। भगवान् सत्य हैं। भगवान् प्रेम हैं। भगवान् सौन्दर्य हैं। भगवान् आनन्द हैं। भगवान् समस्त प्रकाशों के प्रकाश हैं। सभी मनों के मन, प्राणों के प्राण, और समस्त आत्माओं की आत्मा भगवान् हैं। वह आपके हृदय में प्रकाशित हैं और वे आपसे अविच्छिन्न हैं। सदैव उनकी विद्यमानता को अनुभव करें। सदा, सर्वदा, सर्वत्र उनकी विद्यमानता को पहचानने का प्रयत्न करें। चलते-फिरते समय भी उनकी उपस्थिति को अपने साथ-साथ रखें।
२३५
भगवान् ने दुष्ट क्यों बनाये हैं?
क्योंकि यह संसार द्वन्द्वात्मक है, इसलिए यहाँ यदि भले लोग हैं तो दुष्ट भी होंगे ही। कोई भी दुष्ट मनुष्य सदा के लिए दुष्ट नहीं होता। दुर्जन भी भविष्य में सज्जन हो जाता है। दुष्टता एक नकारात्मक गुण है। इससे कुछ भिन्न अस्तित्व इसका नहीं है। यदि दुर्जन न हों तो सज्जनता का, यदि बेईमानी न हो तो ईमानदारी का और यदि दुष्टता न हो तो भलाई का कोई महत्त्व नहीं रहेगा। शठ की सत्ता नेक एवं भले व्यक्ति की महिमा प्रकट करने के लिए है। बेईमानी और ईमानदारी वस्तुतः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों केवल मन की ही रचनाएँ मात्र हैं। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य में भी कुछ-न-कुछ सद्गुण होते हैं। पूर्णतया दुष्टता अथवा पूर्ण रूप से भलाई नहीं होती। अर्थात् कुछ-न-कुछ कमी तो रहती ही है। संसार के रंगमंच पर हो रहे नाटक में भगवान् अपनी लीला हेतु स्वयं ही दुष्ट की भूमिका में लीला करते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई तो है ही नहीं।
२३६
जब मैं स्वर्गाश्रम में था तब आपनी ने मुझसे कहा था कि हमें मुसलिम के हाथों से खाद्य-पदार्थ ले लेने चाहिए और ऐसा करते समय मन में कोई संकोच या दुविधा नहीं आनी चाहिए। किन्तु हमारे शास्त्र हमें यह शिक्षा देते हैं कि पापी के हाथ से खाद्य-सामग्री नहीं लेनी चाहिए। मुसलिम गोमांसभक्षी हैं, उनके हाथों से हमें भोजन क्यों स्वीकार करना चाहिए?
यदि आप यह सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति कुकर्मी है, तो उसके हाथ का भोजन न ग्रहण करें। यदि आपका विचार है कि भगवान् शिव अथवा हरि का कुकर्मी में भी निवास है, यदि आपका यह विचार दृढ़ है, तो आप किसी के भी हाथों से खाद्य-पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अभी आपका दृष्टिकोण अत्यन्त सीमित है। आध्यात्मिक पथ पर अभी आपने चलना प्रारम्भ ही किया है। अभी आपका हृदय विशाल नहीं हुआ है। अभी आप बहुत अधिक जप करें तथा अन्य जो आध्यात्मिक साधनाएँ आपको मैंने सिखायी थीं, उन सबको मन लगा कर करें। 'उनकी' उपस्थिति पाषाण, पुष्प, चम्मच, तौलिये में- प्रत्येक वस्तु में अनुभव करें। कुछ समय के पश्चात् आप उन्नत हो जायेंगे। आप प्रत्येक वस्तु में। केवल भगवान् के ही दर्शन करने लगेंगे। अभी तो आपके हृदय में अत्यन्त मुद्र मुसलिम-विरोधी संस्कार हैं। धीरे-धीरे इन्हें नष्ट कर डालें। किसी मुसलिम को हृदय की गहराइयों से स्नेह करें। भक्तिभाव सहित उसकी सेवा करें। उसके उज्ज्वल नेत्रों में, उसके हृदय की धड़कन में प्रभु को निहारें। सात्त्विक आहार लें। उसे भगवान् को समर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करें। भोजन से पहले भगवन्नाम लें। इस तरह आप किसी भी प्रकार के अशुद्ध आहार का आध्यात्मीकरण कर सकते हैं।
२३७
कहते हैं कि योगाभ्यास केवल पुरुषों के लिए ही है, क्योंकि केवल उन्हें ही संयम अथवा नियन्त्रण की आवश्यकता है। आश्चर्य है कि फिर स्त्रियों के लिए कौन सा कार्य है ? सम्भवतया घर में बैठना और सन्तानोत्पत्ति ही ! किन्तु क्या यह सत्य है कि योगाभ्यास की केवल पुरुषों को ही आवश्यकता है? जैसे पुरुष महान् योगी बनते हैं, क्या स्त्रियाँ इसी प्रकार महान् योगिनी नहीं बन सकर्ती ? अथवा यह स्त्री-लिंग से भी सम्बन्धित है ? आध्यात्मिक महानता और स्त्रियों में यह लिंग-भेद क्यों खड़ा है ?
रानी चुडाला एक महान् योगिनी थीं। उनके पास अनेकों उच्च स्तर की सिद्धियाँ थीं। उन्होंने तो अपने पति शिखिध्वज को भी परिवर्तित कर दिया था और उसे मोक्ष-प्राप्ति में सहायता की थी। योगवासिष्ठ में रानी चुडाला का वृत्तान्त पढ़ कर देखें। स्त्रियों में वैराग्य और तितिक्षा की क्षमता अल्प होती है। उन्हें पुरुषों के समान क्षमताएँ प्राप्त नहीं हैं। इसीलिए महिलाओं में बहुत अधिक योगिनियाँ नहीं बन पायी हैं। महिलाएं भगवान् के दर्शन अधिक सरलता से प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि उनमें स्नेह अथवा प्रेम का तत्त्व अधिक है और इसी कारण भक्ति की भावना का उनमें स्वाभाविक रूप से आधिक्य है। आध्यात्मिक महानता में लिंग-भेद बाधक नहीं है। गार्गी, मदालसा और सुलभा आदि सभी महान् योगिनियाँ थीं।
२३८
ज्ञानी व्यक्ति वस्तु-पदार्थों को किस प्रकार से देखता है? कृपया उसके दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए।
यह वर्णनातीत है। यह व्यक्ति की अपनी भावना है। कभी-कभी आप निद्रावस्था में अपने शरीर को खुजलाते हैं और देह पर बैठने वाली मक्खियों को भी उड़ा देते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है, "क्या तुम्हें स्मरण है कि जब तुम सोये हुए थे तो अपनी देह पर खुजली कर रहे थे, मक्खियाँ उड़ा रहे थे?" आपका उत्तर 'नहीं' में होगा। इसी प्रकार एक ज्ञानी यद्यपि देखता है, तथापि वह नहीं देखता। वह सदैव अपने स्वरूप के प्रति सचेत रहता है। यदि वह चाहता है तो वह दोहरी चेतना रख सकता है और अपनी दृष्टि को उस ओर मोड़ सकता है तथा इस ओर भी पलट सकता है। उसके क्रिया-कलाप एक बालक के समान होते हैं। मानसिक अवधारणा (गत शुभ वासनाओं की शक्ति एवं लेश अविद्या) के कारण उसके क्रिया-कलाप चलते रहते हैं। जैसे हींग अथवा लहसुन के डिब्बे में से उन वस्तुओं को निकाल कर उन्हें कितनी ही बार साबुन एवं गर्म पानी से धो देने पर भी उनमें से वह गन्ध आती रहती है, इसी प्रकार जीवन्मुक्त महापुरुष का भी जब तक प्रारब्ध शेष रहता है, तब तक अविद्या का यह लेश चलता रहता है। अपने दृष्टिकोण से वह किञ्चित् भी कर्म नहीं करता। देखने वाले समझते हैं कि ज्ञानी कर्म कर रहा है। किन्तु हमें यह मानना होगा कि लेश अविद्या यह कार्य कर रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्ञानी खाता, स्नान करता और शौच इत्यादि सभी स्वाभाविक कार्य करता है।
२३९
आपने अपनी शिक्षाओं में से एक में यह कहा है कि साधक को मास में केवल एक बार उपवास करना चाहिए, किन्तु गाँधी जी तथा अन्य कई महापुरुषों ने व्रत-उपवास के ऊपर अत्यधिक बल दिया है और कहा है कि व्यक्ति को मास में कम-से-कम तीन या चार बार निराहार रहना ही चाहिए। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि उपवास आत्म-संयम करने में सहायक है। आप फिर अधिक उपवास करने की आज्ञा क्यों नहीं देते ?
निश्चित रूप से उपवास से आत्म-संयम में सहायता मिलती है, किन्तु अत्यधिक निराहार रहने से देह-मन निर्बल हो कर आध्यात्मिक साधना में बाधक बन जाता है। मैं भी व्रत-उपवास का दृढ़ पक्षपाती हूँ। उपवास एक महान् प्रायश्चित्तकारक है। यह किसी भी प्रकार के पाप से व्यक्ति को अति शीघ्र मुक्त करवा देता है। व्यक्ति के हृदय पर इसका अति गहन शुद्धिकारक प्रभाव पड़ता है। मनुस्मृति का अध्ययन करें। क्योंकि प्रायः अधिकांश लोग व्रत रखने से बहुत भयभीत हो जाते हैं, इसलिए मैंने मास में एक बार उपवास करने के लिये कहा है। युवकों को, स्वस्थ लोगों को, भारी-भरकम शरीर वालों को और जिन्हें काम-वासना अधिक परेशान करती है, उन्हें मास में दो या तीन बार उपवास रखना चाहिए।
२४०
मैं एक आस्तिक व्यक्ति हूँ। किन्तु ऐसा क्यों होता है कि जब मैं सांसारिक लोगों के सम्पर्क में रहता हूँ तो नास्तिक बन जाता हूँ?
आपके आध्यात्मिक संस्कार अभी अधिक सुदृढ़ नहीं हुए हैं। अभी आप पूर्ण रूप से रूपान्तरित नहीं हुए हैं। अभी आपको एक वर्ष तक और अधिक सत्संग की आवश्यकता है। आपको प्रतिदिन किसी भी मन्त्र की दो सौ माला का नित्य जप करना चाहिए। केवल सात्त्विक आहार ही लेना चाहिए जैसे-चावल, दाल, रोटी, फल और दूध। आमिष भोजन का तत्काल त्याग कर दें। नित्य दो घण्टे का मौन रखें। दो घण्टे तक अपने कक्ष में एकान्त में रहें। अन्तर्निरीक्षण करें। ध्यान करें। अपने विचारों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें।
२४१
क्या श्वास के अवरोधन के समय चेतना बनी रहती है? कृपया मुझे व्याख्या सहित समझायें।
हरी सिंह एक हठयोगी था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में उसे एक सन्दूक में बन्द करके धरती के भीतर दबा कर रखा गया। तीन मास बाद जब सन्दूक निकाल कर खोला गया तो वह जीवित बाहर निकल आया। हठयोगी बहिर खेचरी मुद्रा की चलन, दोषन एवं छेदन क्रिया के द्वारा अपने तालुचक्र को अवरुद्ध कर लेते हैं। वे सहस्रार चक्र से टपकते हुए अमृत का अपने तालु से धीरे-धीरे पान करते रहते हैं। हरी सिंह के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक 'मैं' प्राणों से पूर्णतया भिन्न है, श्वास के अवरुद्ध हो जाने पर भी यह चेतना सतत बनी रही है।
२४२
मल और विक्षेप के दूर होने में तो बहुत अधिक समय लगता है। क्या करना चाहिए?
यदि आप विश्वविद्यालय की उच्च कक्षा में पहुँच कर सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने ही वर्ष लग जाते हैं। आपको मैट्रिक और बारहवीं कक्षाओं से उत्तीर्ण हो कर फिर बी.ए. कर लेने के उपरान्त एम. ए. में आना होता है। इसी प्रकार मल और विक्षेप को दूर करने के लिए आपको बहुत दीर्घ समय तक निरन्तर प्रयास करते रहना पड़ेगा। केवल एक मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे को कितने अधिक समय तक टकटकी लगा कर निश्चेष्ट अवस्था में बैठे रहना पड़ता है। जब ऐसी छोटी-छोटी नगण्य-सी वस्तुओं के लिए ऐसा कठिन प्रयत्न करना पड़ता है तब फिर ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति के लिए क्या कहें? यह तो क्षुरस्यधारा - तीक्ष्ण धार वाली तलवार के ऊपर चलने के समान है।
२४३
एक वृत्ति उदित होती है, "मैं अब इस संसार को त्याग दूँ और ऋषिकेश जैसे किसी एकान्त स्थान में रहते हुए भजन करूँ।" तत्काल ही एक अन्य वृत्ति उठती है, "मुझे गृहस्थ-जीवन में रहते हुए जनक की भाँति योग का अभ्यास करना उचित रहेगा।" स्वामी जी, कैसे ज्ञात हो कि अमुक वृत्ति आत्मा से उदित हुई है, अथवा मन से या बुद्धि से उठी है? मैं तो भ्रमित हो गया हूँ।
एक सामान्य सांसारिक मनुष्य के लिए आत्मा की आन्तरिक वाणी को सुन सकना अत्यन्त कठिन है। वह तो विचारों की शुद्ध वाणी को भी सुन नहीं सकता। कोई भी सात्त्विक विचार केवल सात्त्विक बुद्धि से ही उदित होता है। सांसारिक व्यक्ति के समस्त विचार केवल मन से ही उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है और जिसका मन शुद्ध हो चुका है, उसके मन में भगवान् के विचार आने आरम्भ हो जाते हैं। साधारणतया मन में विविध प्रकार के उत्सुकतापूर्ण एवं विचित्र काल्पनिक ख्याल उठा करते हैं। यह सभी को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह विचार उठ रहा है। किन्तु व्यावहारिक रूप से कुछ करने का समय आने पर यह कुछ भी नहीं करेगा। यदि आप एकाग्रता और ध्यान करने के लिए गम्भीरतापूर्वक दृढ़-प्रतिज्ञ हैं और यदि आप महीनों पर्यन्त इसके अभ्यास में लगे रहते हैं, और यदि आपकी प्रभु-दर्शन अथवा आत्म-साक्षात्कार की इच्छा अति तीव्र हो जाती है, केवल तभी समझें कि इस प्रकार के समस्त विचार आपकी केवल सात्त्विक बुद्धि से उदित हो रहे हैं।
२४४
क्या आप कृपा करके मुझे अपने प्रत्येक कार्य में मन की अनासक्ति बनाये रखने सम्बन्धी कुछेक विस्तृत व्यावहारिक बिन्दु बतला देंगे?
प्रत्येक कार्य करते समय अपने मन में यह भाव रखें कि आप भगवान् के हाथों के एक उपकरण हैं अर्थात् निमित्त मात्र हैं। इससे अहंकार और सम्मान प्राप्ति की भावना नष्ट हो जायेगी। अपने किये गये कार्य के लिए फल-प्राप्ति की इच्छा न रखें अर्थात् निष्काम भावना से कार्य करें। आप कार्य के फल को प्राप्त करने की इच्छा कर भी कैसे सकते हैं जब कार्य करने वाले तो कोई अन्य अर्थात् परमात्मा हैं जो कि आपके माध्यम से स्वय कार्य करते हैं? और जब आप यह जानते हैं कि यह संसार दुःखों से भरा हुआ है तब फिर यहाँ फिर से लौट कर आने का क्या लाभ है? आप भगवान् के हाथों की एक कठपुतली भर हैं जिसका धागा उनके हाथों में है। वे ही सूत्रधार हैं। अपने समस्त कार्य कर्तव्य-भावना से करें। अपनी आवश्यकताओं को कम कर दें। अत्यन्त सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करें। ऐश्वर्य-भोग से घृणा करें। इन्द्रियों का दमन करें। संसार के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु को भगवान् का प्रकटीकृत रूप समझें। ऐसा विचार बनाये रखे कि यह संसार भ्रान्ति और एक दीर्घ स्वप्नवत् है। तब फिर संसार में आसक्ति कैसे होगी, मेरे प्यारे रामचन्द्र? यदि आप इस प्रकार कार्य करेंगे, तो आप व्यावहारिक योगी बन जायेंगे। मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूँ। अपने मन में आनन्दित हो जायें। अपनी कमर कस लें और दैनिक जीवन के युद्ध में वीरता सहित निर्भय हो कर लग जायें।
२४५
भगवान् मुझे दुष्कर्म की ओर क्यों लगाते हैं?
भगवान् कभी भी आपको दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं करते। वे सदैव साक्षी अथवा द्रष्टा हैं। आपका अपना स्वभाव, आपके अपने कुसंस्कार ही आपको ऐसे कार्य की ओर बलात् प्रवृत्त कर देते हैं। 'स्वभावस्तु प्रवर्तते' - यह गीता का कथन (अ. ५-१४) है। आपमें विवेक का अभाव है। यही कारण है कि आप मनोवेगों के दास बन जाते हैं। मनोविकारों को नियन्त्रित करने के लिए भगवान् ने आपको बुद्धि दी है। तब फिर आप इसका उपयोग क्यों नहीं करते?
२४६
मैं कभी भी कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहता। फिर भी जब कभी ऐसा हो जाता है तो क्या यह मेरा उत्तरदायित्व होगा? यदि ऐसा है तो क्या भगवान् मुझे क्षमा कर देंगे? यदि वे क्षमा कर देंगे तो उस कर्म का क्या फल होगा ? मैं आपको निश्छल हृदय से यह लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपना करुणाशील निर्देशक माना है। कृपया मुझे क्षमा कर दें और मेरी सहायता करें।
निःसन्देह आप अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान् कभी क्षमा नहीं करते। कर्म अपना फल स्वयं लाता है। प्रायश्चित्त के द्वारा आप अपने अनुचित कर्म के कुप्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में प्रायश्चित्त करते समय आप कष्ट भोग लेते हैं, अतः उस कर्म का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वह अनुचित कर्म आपके आगामी जन्म में आपके साथ नहीं आता। निश्छलता एवं गम्भीरतापूर्वक किया गया प्रायश्चित्त, जप, उपवास और दान, किये गये अनुचित कर्म के कुप्रभाव को नष्ट कर देते हैं। पश्चात्ताप में भोगे गये कष्ट से अनुचित कर्म का प्रभाव धुल जाता है। प्रायश्चित्त अनुतापी-हृदय से किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से आपको अनुचित कर्म पुनः कभी नहीं करना चाहिए।
२४७
विभिन्न पीर-पैगम्बर अथवा अवतारी पुरुष परस्पर विरोधी शिक्षाएँ क्यों देते हैं?
अवतारी पुरुष समय-समय पर अधर्म का विनाश तथा धर्म की स्थापना हेतु इस धरा पर आया करते हैं। वे सब समय, स्थान, परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देते हैं। भगवान् बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश देते हुए कहा, "किसी की भी हत्या न करो।" गुरु गोविन्द सिंह जी ने कहा, "मार डालो।" जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तब लोगों में पशु-बली देने का अत्यधिक प्रचलन था। उन्होंने हत्या को रोकने के लिए अहिंसा का उपदेश दिया। गुरु गोविन्द सिंह जी ने लोगों में वीरता का संचार करना था। एक पैगम्बर ने उपदेश दिया, "सब-कुछ त्याग कर वन-गमन करो।" श्री रामानुजाचार्य ने शिक्षा दी, “घर में रहो। आसक्ति त्याग कर सुख भोग करो। भगवान् विष्णु की आराधना करो।" वास्तव में शिक्षाएँ परस्पर विरोधी नहीं हैं। अवसर, समय और मानव-स्वभाव के अनुसार तब उनकी ही आवश्यकता होती है।
२४८
भगवान् ने कुछ को शुद्धात्मा सम्पन्न और कुछ को दुष्टात्मा क्यों बनाया है ? किन्हीं लोगों को भगवान् दुष्कर्मों में लगा कर अच्छा बनने से क्यों रोकतेहैं? मुझे परिपूर्णता कब प्राप्त हो सकती है?
दीर्घकालीन संघर्ष के द्वारा आप परिपूर्णता और अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। नश्वर प्राणी इस सापेक्ष जगत् में आ कर भले और बुरे, दोनों प्रकार के कर्म करता है। बुराई भी नकारात्मक भलाई ही है। कई बार बुराई में से भलाई का जन्म हो जाता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति पाठ सीखता है और विकसित होता है। भगवान् तो केवल द्रष्टा हैं। वे मनुष्य से दुष्कर्म नहीं करवाते। मनुष्य के पास बुद्धि और कर्म करने की स्वतन्त्र सामर्थ्य है। मनुष्य अहंकारवश अपनी इच्छानुसार कर्म करता है और फिर अपने दुष्कर्मों का फल भोगता है। जब भले कर्मों के द्वारा सत्त्व अथवा पवित्रता की वृद्धि होती है, तब वह दिव्य बन जाता है। भले या बुरे, किसी भी कर्म के लिए भगवान् उत्तरदायी नहीं हैं।
२४९
आप कहते हैं कि क्षमा का व्यावहारिक रूप से अभ्यास करना चाहिए। अपने कार्यालय में सर्वोच्च पदाधिकारी न होने के कारण अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के दण्डित होने में मैं रक्षा नहीं कर सकता। यदि मैं उनकी गलतियों को छुपाऊँ तो अपने कर्तव्य-निर्वाह में पूर्ण नहीं उतरूँगा और इस प्रकार किसी दिन मुझे भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रतिवेदन भेजता हूँ तो उन्हें दण्ड दिया जाता है और मुझे इससे कष्ट अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ ?
अपने सेवकों एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की छोटी-छोटी गलतियों को आप क्षमा कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। अपने मन को शुद्ध रखें। जब भी वे गलती करें तो उसी समय उन्हें चेतावनी दे दें। आप व्यावहारिक क्षेत्र में हैं, गम्भीर गलती करने वालों को आपको दण्ड देना ही पड़ेगा। किन्तु पक्षपात की प्रवृत्ति से बचें। भगवान् का भय मानें। यदि निर्धन सेवकों को धन का दण्ड लगाया जाता है तो उन्हें अपनी ओर से कुछ वित्तीय सहायता कर दें। उनसे प्रेम करें। भविष्य में वे पुनः गलती नहीं करेंगे।
२५०
क्या मैं जान सकता हूँ कि एकाग्रता की शक्ति को कैसे विकसित किया जाता है?
अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को कम करने से, प्रतिदिन दो घण्टे का मौन रखने से, प्रतिदिन एक या दो घण्टे तक अपने कक्ष में एकान्त में रहने से, प्राणायाम का अभ्यास करने से, प्रार्थना करने से, सायंकाल और रात्रि में भी ध्यान की अवधि एवं ध्यान के लिए बैठने की संख्या में वृद्धि कर देने से तथा विवेक सहित विचार करने से एकाग्रता को विकसित किया जा सकता है।
२५१
यह कैसे सम्भव है कि सृष्टिकर्ता, जो प्रेम से परिपूर्ण है, उसने ऐसी सृष्टि और ऐसी प्रकृति की रचना की जहाँ पशु-पक्षी केवल अन्य पशु-पक्षियों का भक्षण करके ही जीवित रह सकते हैं कि उनको इतना दुःख एवं कष्ट सहन करना पड़ता है? कोई भी मुझे इसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता।
यदि मनुष्य एक-दूसरे की हत्या करते हैं तो यह पाप है, उन्हें ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। किन्तु इतर प्राणियों को अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों की हत्या करनी ही पड़ती है। आप क्या कहते हैं? हम आपका विचार जानने के लिए उत्सुक हैं।
इस विश्व के प्रति भगवान् को असीम प्रेम है, सृष्टि के प्राणियों के अनुभवों के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। भगवान् निजी रूप में किसी को किसी भी प्रकार से दण्डित अथवा पुरस्कृत नहीं करते, यह तो मनुष्य के अपने पाप अथवा पुण्य-कर्म होते हैं जो यहाँ के अनुभवों का कारण बनते हैं।
मानव क्योंकि नैतिकता के बोध से सम्पन्न है और उसको कर्तृत्व एवं उत्तरदायित्व का बोध भी प्रदान किया गया है, इसलिए वह मानवेतर जीवों के कर्मों पर भी यह नैतिकता एवं उत्तरदायित्व की भावना को थोपता है। इसलिए दोष मनुष्य का है, उन पशु-पक्षियों का नहीं जो बिना नैतिकता के बोध के, स्वाभाविक रूप से तथा कर्तृत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना रहित हो कर कर्म करते हैं।
कोई भी कर्म तब तक प्रतिफलात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं करता जब तक व्यक्तिगत कर्तृत्व और उत्तरदायित्व की भावना से न किया गया हो। मानव को क्योंकि कर्म करने की स्वतन्त्रता और किये गये के उत्तरदायित्व की सामर्थ्य दी गयी है इसलिए वह प्रतिफलात्मक न्याय द्वारा दण्डित होगा। किन्तु मानवेतर जीवों को ऐसी स्वतन्त्रता और सोचने-समझने की क्षमता प्रदान नहीं की गयी, इसलिए वह जो कुछ भी करते हैं वह केवल उनकी नैसर्गिक अथवा सहज-स्वाभाविक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति मात्र ही है और यह वैश्व प्रकृति के नियमानुकूल है। प्रकृति नैतिकता के नियमों से अतीत है। नैतिक व्यवहार केवल मानव के लिए, उसके व्यवहार को नियन्त्रण में रखने और इस प्रकार विकास के सोपान के द्वारा उसे वैश्व चैतन्य की ओर अग्रसर करने के लिए है।
जो जन्मा है, उसकी मृत्यु निश्चित है और इस विनाश के लिए कोई-न-कोई तात्कालिक कारण भी होना चाहिए। इस विनाश का कारण कोई अन्य पशु, भूकम्प, बादल फटना, बाढ़, रोग, तूफ़ान अथवा अन्य ऐसा कुछ भी हो सकता है। इनको तब तक नैतिकता के मूल्यों से आवृत नहीं करना चाहिए जब तक किसी मनुष्य का इनके करने से कोई सम्बन्ध न हो।
२५२
कभी-कभी मैं कई बातों को अपने मन में ही गुप्त रख लेता हूँ और फिर उसके कारण अत्यन्त मानसिक यातना से ग्रसित हो जाता हूँ। अपने इस स्वभाव को बदलने के लिए मैं क्या करूँ ?
आपको निश्चित रूप से शिशु की भाँति स्पष्टवक्ता एवं सरल होना चाहिए। केवल तभी आपको दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो सकेगी। तब ही आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। भले ही कोई भयंकर अपराध किया हो, तो भी उसे अपने गुरु के समक्ष स्वीकार कर लें। केवल तभी आपको गुरु से सहानुभूति और सुरक्षा प्राप्त होगी। दूसरों के समक्ष अपने दोष स्वीकार कर लेने से आप दुष्कर्मों के कुप्रभाव को दूर कर लेते हैं। यह प्रायश्चित्त कर लेने जैसा कार्य करता है।
२५३
मौन-व्रत करने के क्या लाभ हैं, क्या यह मुझे भी करना चाहिए?
अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय नित्य कुछ घण्टे मौन व्रत का पालन करें। शेष समय भी अति अल्प बोलने का ही प्रयत्न करें। अनावश्यक वार्तालाप से दूर रहें। कठोर शब्द और अश्लील भाषा का प्रयोग न करें। मधुरता एवं कोमलता सहित बोलें। आपको अपनी वाणी पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। वाणी पर नियन्त्रण का अर्थ है-मन पर नियन्त्रण। वाक् इन्द्रिय मन को अत्यधिक विकर्षित करती है। मौन आपको शान्ति प्रदान करता है। यह तनाव और कलह से बचाता है। यह आपकी मानसिक शक्ति को विकसित करता है। यह आपकी शक्ति को सुरक्षित रखता है। यह विचार-प्रवाह को कम करता है।
२५४
क्या जीवन्मुक्त भी पुनः जन्म लेगा ?
कुछ जीवन्मुक्त जिनके हृदय करुणा और व्यवहार अपेक्षा से आपूरित होते हैं, जैसे बौद्ध अर्हतों के, वे स्वेच्छा से जन्म ले लेते हैं-जैसे श्री शंकराचार्य, श्री दत्तात्रेय अथवा श्री ज्ञानदेव। जन्म से ही सिद्ध होने के कारण उन्हें कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। वे तो आध्यात्मिक दिव्य प्रकाश-पुञ्ज के रूप में अचानक प्रकट होते हैं, कुछ आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, कतिपय मूल्यवान् दार्शनिक पुस्तकें लिखते हैं, किन्हीं बड़ी विपत्तियों को दूर कर देते हैं, अति शीघ्र देह त्याग देते हैं और फिर ब्रह्मलीन हो जाते हैं (विदेह कैवल्यम्)। वे सब अंशावतार होते हैं जो स्वयं में विशेष ईश्वरीय कला लिये होते हैं।
२५५
ईश्वरानुभूति प्राप्त दिव्यात्माएँ नश्वर देह को त्यागने के उपरान्त ब्रह्म में लीन हो जाती हैं और फिर उनका किसी भी लोक में कोई निजी व्यक्तित्व नहीं रहता। तथापि ऐसा माना जाता है कि साई बाबा अथवा उनके जैसे अन्य सन्त, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, अपने उन भक्तों को सहायता एवं निर्देशन प्रदान करते हैं जो उनसे आशीर्वाद पाने के आकांक्षी हैं। इस विरोधाभासी प्रतीत होने वाली बात को कैसे समझा जाये ?
जो आत्म-साक्षात्कार प्राप्त दिव्यात्मा भौतिक शरीर को त्याग देने के उपरान्त भी अपने उन भक्तों की सहायता करना चाहते हैं जिन्हें सहायता की अत्यन्त आवश्यकता होती है, वे अपने सूक्ष्म शरीर को रख लेते हैं। किन्तु जीवन्मुक्त सामान्यतया मात्र साधकों की सहायता करने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर को नहीं रखते, क्योंकि इस संसार में भी सदैव ऐसे उन्नत महान् आत्मा रहते ही हैं जो आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान करने का कार्य करते रहें।
२५६
कई बार मुझे लगता है कि मैं माया के पाश में उलझ गया हूँ और स्वयं को उससे विमुक्त करने का प्रयास करता हूँ। और कभी यह अनुभव करता हूँ कि मैं नित्य शुद्ध, बुद्ध, अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ। मैं आपकी उस कृपा का अभिलाषी हूँ जो मुझे निश्चित रूप से इस दुःखमय भव-सागर से पार ले जायेगी। मेरे लिए कोई निर्देश ?
आप संघर्षपूर्ण स्थिति में हैं। निस्सन्देह आप उन्नति की ओर अग्रसर हैं। शीघ्र ही आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जायेंगे। भयभीत न हों। लगे रहें। निरन्तर परिश्रम करते रहें। पीछे पलट कर न देखें। निर्भीकता सहित आगे बढ़ते जायें। लक्ष्य अत्यन्त निकट है। अपने समस्त कार्यों के साक्षी मात्र बन कर रहें। आप असंग, अकर्ता हैं। आप अमर आत्मा हैं।
२५७
गत तीन वर्ष से मैं आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी उन्नति हो रही प्रतीत नहीं होती। ऐसा क्यों?
उन्नति तो हुई है। आपके मानसिक प्रतिबिम्ब अब सुदृढ़ एवं स्थिर हो गये हैं। स्मरण रखें कि आध्यात्मिक जगत् में आध्यात्मिक उन्नति को मापने के लिए कोई भार-मापक अथवा ताप-मापक यन्त्र नहीं होता। अभी आप भगवान् को अपना आधा ही मन दे रहे हैं। मन की चहुँओर बिखरी हुई तरंगों को एकत्रित करें और अपना पूरा-का-पूरा मन भगवान् को दे दें। मैं आपको सुनिश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ, 'आप इसी क्षण उन्हें पा लेंगे।'
२५८
मुझे हर तरह से कठिनाइयाँ और चिन्ताएँ व्याकुल करती हैं। असफलताएँ और मुसीबतें हर ओर से मुझे घेर लेती हैं। पारिवारिक कर्तव्य मेरी साधना में बाधा डालते हैं। मेरे प्रभु, मैं क्या करूँ ?
भयभीत न हों। इस कथन को स्मरण रखें, 'यह भी बीत जायेगा।' इसे एक कागज़ के टुकड़े पर बड़े-बड़े और मोटे अक्षरों में टाइप कर लें और अपने कक्ष की दीवार पर चिपका दें। कठिनाइयाँ और मुसीबतें आगमापाय हैं। यह आने और जाने वाली हैं। गीता के द्वितीय अध्याय के १४ वें श्लोक को पढ़ें। वीर-नायक बनें। चट्टान की भाँति सुदृढ़तापूर्वक खड़े रहें। आत्म-केन्द्रित रहें। ॐ में निवास करें। सत्य या आत्मा में निवास करें। कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। कठिनाइयाँ आपको और भी अधिक सुदृढ़ बना देंगी तथा आपको और अधिक सहनशक्ति प्रदान करेंगी। भगवान् के मार्ग निराले हैं। सदा यही कहें, 'आपकी इच्छा पूर्ण होगी!'
२५९
हम प्रायः देखते हैं कि इस संसार में दुष्ट लोग तो फल-फूल रहे हैं किन्तु भले व्यक्ति कष्ट भोगते हैं, ऐसा क्यों? भगवान् किसी के लिए दयालु और किसी के प्रति निष्ठुर क्यों हैं?
यह प्रश्न शताब्दियों से चला आ रहा है, यह उतना ही पुराना है जितना कि यह संसार। महान् भीष्म जब मृत्यु-शैया पर थे तो उनके अश्रु प्रवाहित होने लगे। जब उनसे रोने का कारण पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि पाण्डव भगवान् के गहन भक्त थे और सदैव धर्म के पथ पर चलते थे। सबसे बढ़ कर यह कि श्री कृष्ण के रूप में भगवान् सदैव उनके साथ रहे। और फिर भी उन्हें इतने अधिक कष्ट सहने पड़े।
कई दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति इस दम्भपूर्ण संसार में समृद्ध दिखायी देते हैं, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे कष्टों से मुक्त हैं। वास्तव में भले लोग उतना कह नहीं भोगते जितना 'समृद्ध' दुष्ट व्यक्ति, क्योंकि सज्जन व्यक्तियों के हृदय में शान्नि होती है। आदर्शों का पालन करने की योग्यता प्राप्ति के लिए वे सदा पवित्र रहते हैं जो कि अपने-आपमें प्रसन्नता के महान् स्रोत हैं। लोगों के सुखों और दुःखों की व्याख्या केवल कर्म के सिद्धान्त के आधार पर ही हो सकती है।
भले लोग कष्ट भोगते हैं क्योंकि गत जन्मों में उनसे कोई अनुचित कार्य हो गया होता है। दुष्ट लोग, जो समृद्ध दिखायी देते हैं, वे अपने गत जन्मों में किये गये पुण्यों का फल भोगते हैं, किन्तु उन्हें वर्तमान जीवन में किये जा रहे कुकर्मों का फल बाद में अवश्य भोगना पड़ेगा। यह कर्म का सिद्धान्त है जो मनुष्य की समस्त भली और बुरी परिस्थितियों का कारण है। यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को अच्छी अथवा खराब करने का या उसे सुखी अथवा दुःखी करने का कारण भगवान् होते, तब तो उनका भगवान् होना ही व्यर्थ हो जाता; क्योंकि ऐसे पक्षपाती भगवान् जो अकारण ही किसी के साथ भला और किसी के साथ अनुचित करें, वह तो भगवान् ही नहीं हो सकते।
२६०
एक ज्ञानी, जब वह सुस्वादु आम अथवा कोई अन्य स्वादिष्ट वस्तु खा रहा होता है, तब उसके मन में कैसे भाव उठते हैं?
उसके मन में भोक्ता, भोग और भोग्य के विचार नहीं होते। आम खाने का कोई संस्कार उसमें उत्पन्न नहीं होता। किसी अन्य समय में उसके मन में यह विचार नहीं उठता, 'मैंने गत वर्ष श्री रमन के बंगले पर कितना स्वादिष्ट आम खाया था।' उसे कर्म सकल्प नहीं होता। वह 'अहम् भोक्ता' के भाव से मुक्त होता है। उसे क्षुधा का बोध होता है। वह जानता है कि क्षुधा प्राणमय कोष का धर्म है और क्षुधा-पूर्ति हेतु कोई-न-कोई खाद्य-पदार्थ आमाशय में पहुँचाना चाहिए।
२६१
इस धरा के दूसरे गोलार्ध की दूरी से क्या आप मेरे जीवन के लक्ष्य के विषय में मुझे बता सकते हैं?
आपके जीवन का लक्ष्य है, अपनी इन्द्रियों की समस्त शक्तियों से भगवान् के प्रति समर्पित हो जाना और इस सम्बन्ध में कोई उत्सुकता न रखना कि वे आपका उपयोग किस प्रकार से करेंगे। उन्होंने अकारण ही हमसे अपने उच्चतर उद्देश्यों को गुप्त नहीं रखा है। हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में हमारा सीमित मन कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए वे पहले कुछ भी अनावृत नहीं करते और हमें यह जानने की उत्सुकता रखने की आवश्यकता भी नहीं है। स्वयं को उनके समक्ष पूर्णतया समर्पित कर दें। उन्होंने आपका पहले से ही चयन कर रखा है और वे समय-समय पर आपको कार्यभार सौंपते रहेंगे, आप उन्हें निःस्वार्थ भाव से करते जायें तथा दिव्य सेवा में उच्च से उच्चतर विकसित होते रहें। यही आपका भगवान् के प्रति और उनकी रचना, इस सृष्टि के प्रति काया, वाचा, मनसा प्रेम का यथार्थ प्रकटीकरण होगा।
२६२
क्या यह सत्य है कि मृत्यु (स्वैच्छिक या अन्य प्रकार से) हमें आगामी जन्म में उन कतिपय प्रसुप्त तीव्र इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, जिनकी अन्यथा पूर्ति हो सकना अति कठिन होता ?
यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु से मनुष्य को आगामी जन्म में अधिक अनुकूल वातावरण अथवा परिस्थितियाँ प्राप्त हों। यह तो उसके वर्तमान जीवन के और उससे भी पूर्व के कर्मों की योग्यता पर निर्भर करता है। हाँ, यह सत्य है कि हमारी इच्छाएँ बहुत सीमा तक हमारे भविष्य के जन्मों को निर्देशित करती हैं।
२६३
योगासनों में से कौन से आसन हैं जो विवाहित महिलाओं को अधिक काल तक अपनी युवावस्था को बनाये रखने में सहायक हो सकते हैं?
सर्वांगासन, मत्स्यासन, शीर्षासन, पद्मासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन और चक्रासन तथा साथ में योग मुद्रा और विपरीतकरणी मुद्रा शारीरिक एवं मानसिक सन्तुलन
बनाये रखने में अत्यन्त सहायक हैं। इन सभी को एक-साथ करना अनिवार्य नहीं है। इनमें से जो भी सुविधाजनक लगें, उनका अभ्यास किया जा सकता है, साथ ही अपने स्वास्थ्य की सीमानुसार प्राणायाम करना चाहिए। इन्हें अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयत्न
नहीं करना चाहिए। योगाभ्यासी-पुरुष अथवा महिला जो भी हो-को अपनी वासना-पूर्ति की इच्छा को संयमित करना आवश्यक है।
२६४
हिन्दू भगवद्गीता को 'उत्तर-गीता' से अधिक महत्त्व क्यों देते हैं?
भगवद्गीता में दर्शन की व्याख्या तथा भगवान् श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अधिक व्यापक एवं विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, यह हिन्दू धर्मग्रन्थों में एक महान् कृति है, अतः विषय-वस्तु एवं प्रयोजन में यह भगवान् श्री कृष्ण ही की 'उत्तर- गीता' से अधिक महत्त्वपूर्ण है। परन्तु कृपया ध्यान दें कि इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी गीताएँ हैं जैसे कि 'अनु गीता', 'अवधूत गीता' इत्यादि, जो कि सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए सहायक हैं। तथापि विस्तृत एवं लघु दोनों को मिला कर इन दर्जनों से भी अधिक गीताओं में से भगवद्गीता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण, समग्र, व्यापक एवं सर्वोत्तम है।
२६५
मेरे विचार से एक साधक की सबसे बड़ी भूल, जो वह प्रायः कर बैठता है, यह है कि वह भ्रमवश निम्न समाधि को उच्चतर अथवा उच्चतम समाधि समझ लेता है। किन्तु जो व्यक्ति ऐसी भूल कर रहा है, वह ऐसा न करने से अपनी रक्षा कैसे करे?
जब व्यक्ति समाधि की उच्चावस्था पर पहुँच जाता है, तब उससे यह संशय करने की भूल नहीं होती कि वह निम्न समाधि है अथवा उच्चतर या उच्चतम है। वह स्वाभाविक रूप से निःसन्देह जानता है कि वास्तव में क्या है।
२६६
आध्यात्मिक उन्नति के क्या चिह्न हैं? व्यक्ति को कैसे ज्ञात हो कि वह
आध्यात्मिक पथ पर उन्नत हुआ है अथवा नहीं?
प्रत्येक परिस्थिति में मन में शान्ति, प्रसन्नता, वैराग्य, निर्भयता की स्थिति का बने रहना और कभी भी विचलित न होना, यह सब सूचित करता है कि आप आध्यात्मिक पथ में उन्नति कर रहे हैं।
आध्यात्मिक उन्नति सिद्धियों अथवा शक्तियों की उपलब्धि से नहीं अपितु ध्यान की अवस्था में आनन्दपूर्ण स्थिति से नापी जाती है। आध्यात्मिक उन्नति के ये सब सुनिश्चित परीक्षण हैं :
क्या आन्तरिक आध्यात्मिक प्रक्रिया और बाह्य साधना में आपकी रुचि में नित्यप्रति वृद्धि हो रही है?
क्या आपके अन्तर्मन में आध्यात्मिक जीवन का अर्थ, अत्यधिक प्रसन्नता से, सांसारिक सुविधाओं से प्राप्त होने वाले सुखों से कहीं अधिक बढ़ कर आनन्दप्रदायक जीवन से है?
क्या आपकी व्यक्तिगत जागरूकता उस प्रशान्ति और क्षमता को प्राप्त कर सकी है जिसे सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन में नहीं पाते ?
क्या आप यह निश्चित रूप से अनुभव करने लगे हैं कि आपकी विवेक-शक्ति और विचारों में ज्ञान का प्रकाश स्थिरता सहित बढ़ रहा है?
क्या आपके जीवन में ऐसे अनुभव होने लगे हैं जो आपके समक्ष आपसे भिन्न, एक अन्य सत्ता की, सर्वशक्तिमान् परमात्मा की विद्यमानता को प्रकटीकृत करने वाले हों?
और क्या आपके दैनिक जीवन में, एक नवीन आनन्दमय दृष्टिकोण में, एक नूतन सन्दर्भ में, सर्वव्यापक भगवान् पर अपनी निर्भरता एवं उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध की आपकी धारणा में, सुस्थिर रूप से वृद्धि हो रही है?
यदि इन सब प्रश्नों अथवा इनमें से किसी एक का उत्तर 'हाँ' में है, तो पूर्णतया सुनिश्चित है कि आध्यात्मिक पथ पर आपकी उन्नति हो रही है और द्रुत गति से हो रही है।
२६७
इस शरीर के छूटने के उपरान्त जब जीव का अन्य शरीर में पुनः जन्म हो जाता है, तब क्या यह आवश्यक रह जाता है कि हम उसके लिए श्राद्ध-कर्म करें? अब, जब कि वह स्वर्ग में है ही नहीं तो हमारी दी गयी आहुतियाँ किसे प्राप्त होंगी ?
हमारे पित्रों का बहुत दीर्घ समय तक स्वर्ग में, पितृलोक में अथवा चन्द्रलोक में वास रहता है। श्राद्ध-क्रिया से पित्रों के स्वर्गलोक के सुखों में और दिवंगत आत्मा की
शान्ति में वृद्धि होती है। इसी प्रकार दिवंगत आत्मा के अन्य लोकों के कष्ट भी, उनकी सन्तान द्वारा किये गये श्राद्ध-कर्म से अल्प हो जाते हैं। अतः दोनों ही प्रकार से श्राद्ध-कर्म अत्यन्त सहायक है।
और यदि व्यक्ति का मृत्यु के बाद तत्काल पुनः जन्म हो भी जाता है, जैसा कि बहुत ही असाधारण घटनाओं में होता है, तब भी उसके लिए किये जाने वाला श्राद्ध-कर्म, उसके नये जीवन में प्रसन्नता की वृद्धि करता है। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने माता-पिता और पूर्वजों का श्राद्ध करे। यह श्राद्ध-क्रिया अत्यन्त श्रद्धा एवं विश्वास सहित आजीवन करते रहनी चाहिए। धर्म का मुख्य आधार विश्वास है।
शास्त्रों द्वारा मानवता पर लागू किये गये विभिन्न धार्मिक कृत्य अज्ञानी मनुष्य की चित्त-शुद्धि हेतु किये गये हैं। श्राद्ध-कर्म, जो कि शास्त्रानुसार मनुष्य के लिए अवश्य- करणीय कर्मों में से एक है, भी मानव-मन की शुद्धि के लिए है। इसके साथ ही, हमारे पूर्वज भी इससे प्रसन्न होते हैं और उनकी शुभ कामनाओं एवं आशीर्वादों से हमारी भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है।
२६८
कुण्डलिनी जाग्रत करने के लिए व्यक्ति को शीर्षासन अथवा पश्चिमोत्तानासन या कुम्भक अथवा महामुद्रा कितने समय तक करने चाहिए? योग सम्बन्धी किसी भी पुस्तक में यह बताया हुआ नहीं है।
यह सब शुद्धता के स्तर पर, विकास की अवस्था पर, नाड़ियों और प्राणमय कोष की शुद्धि के स्तर पर तथा वैराग्य एवं मुमुक्षुत्व के स्तर पर निर्भर करता है।
विद्यार्थी अपनी साधना का प्रारम्भ उस बिन्दु अथवा स्तर से करता है, जहाँ पर अपने विगत जन्म में उसने छोड़ी होती है। कई तो अपने पूर्व-जन्म में आवश्यक अनुशासन एवं अन्य अभ्यास के द्वारा मन की पूर्ण शुद्धता को ले कर ही जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होते हैं। गुरु नानक, आलन्दी के ज्ञानदेव, वामदेव और अष्टावक्र सभी अपनी बाल्यावस्था में ही दक्ष थे। गुरु नानक जब अभी छोटे बालक ही थे, तो उन्होंने विद्यालय में अपने अध्यापक से ॐ के महत्त्व के विषय में प्रश्न किया था। वामदेव ने अपनी माँ के गर्भ में से ही वेदान्त पर प्रवचन दिये थे।
२६९
मैं भगवान् शिव का भक्त हूँ। क्या मुझे भगवान् विष्णु और देवी माता के मन्दिरों में भी जाना चाहिए? और यदि मैं जाऊँ, तो मुझे वहाँ उन विग्रहों की कैसे पूजा करनी चाहिए?
हाँ, जिस किसी भी मन्दिर में जा सकने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाये, वहाँ जा कर दर्शन करने और पूजा करने का सुअवसर कभी न छोड़ें। यदि वह देवी माँ का अथवा विष्णु भगवान् का मन्दिर हो तो उनमें भी भगवान् शिव को देखते हुए, भगवान् शिव को ही इस रूप में देखते हुए, उनकी पूजा करें। यदि आपके पिता जी उच्चन्यायालय के जज के वेश में आ खड़े हों अथवा किसी नाटक के पात्र के रूप में महिला की पोशाक में आ जायें, तब क्या आप उनसे मुख मोड़ लेंगे? हर रूप और हर पोशाक में आप उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम ही करेंगे। भगवान् की पूजा के समय आपका यही दृष्टिकोण होना चाहिए। भगवान् तो एक हैं। भिन्न-भिन्न लोग उनकी विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं।
२७०
स्वामी जी, यहाँ भारत में लोग जिस प्रकार गुरु की पूजा करते हैं, उसका क्या औचित्य है? क्या यह दासता अर्थात् गुलामी नहीं है? क्या आप यह मानते हैं कि शिष्य अपने गुरु का दास बन जाता है?
क्या आप उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ नहीं होते जो आपकी सहायता करता है, सेवा करता है? आप क्या किसी-न-किसी रूप में उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं करते? यदि आप किसी छोटे से सांसारिक कार्य में सहायता करने वाले व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उसके प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए, जो आपको परमात्मा की ओर का पथ दर्शाता है? उसने आपको नव-जीवन ही नहीं, अमरत्व और शाश्वत आनन्द प्रदान किया है। क्या आप उसे कृतज्ञता प्रकट नहीं करेंगे? गुरु की साक्षात् पूजा करनी, इस सर्वोच्च कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने की भारतीय विधि है। आप उस व्यक्ति को जिसने कुछ दे कर आपकी सहायता की हो, कुछ भेंट दे कर धन्यवाद प्रकट करते हैं, और गुरु, जिसने आपको आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट उपहार प्रदान किया है, उसे आप अपना सर्वस्व दे देते हैं!
यह दासता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को कभी भी अपना दास नहीं बनाता। वस्तुतः गुरु अपने शिष्य का सेवक होता है। वास्तविक गुरु के हृदय में शिष्य के लिए उच्चतम प्रकार का प्रेम होता है। गुरु उसके हृदय में निवास करता है, गुरु अपने शिष्य के मन को जीत लेता है, दोनों अब एक ही हो जाते हैं। दोनों में परस्पर दिव्य प्रेम की भावना होगी-दासता की नहीं।
२७१
एक व्यक्ति, जिसके मन में दीर्घ काल से नकारात्मक विचार निवास कर रहे हों, वह उन्हें सकारात्मक चिन्तन में कैसे परिवर्तित कर सकता है?
उसे चाहिए कि पहले कुछेक ऐसे अर्थगर्भित सकारात्मक सूत्रों से प्रारम्भ करे 'मैं पूर्णतया सुस्वस्थ हूँ। मैं निरोग हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे अपनी योग्यता और क्षमता का सही अनुमान नहीं था। अब मुझे अपनी वास्तविक प्रकृति का बोध हो गया है।' यह सब उसे योग में उन्नत व्यक्ति अथवा किसी भगवद्भक्त की सहायता से करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह भगवान् की प्रार्थना के साथ इसे प्रारम्भ करे। प्रार्थना को तो उसे अपने दैनिक जीवन का अंग, एक 'अति आवश्यक अंग' बना लेना चाहिए। समस्त नकारात्मक चिन्तन समाप्त हो जायेगा और वह पूर्णतया सामान्य हो जायेगा।
२७२
अखण्ड कीर्तन करने का क्या उद्देश्य है?
कीर्तन करने से व्यक्ति के भीतर दिव्य स्पन्दन उत्पन्न होंगे और ये स्पन्दन इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनमें मनुष्य के मन को विकर्षित करने वाली सभी बाह्य शक्तियों को नष्ट कर देने की तथा चंचल मानव-मन को बाँध देने की शक्ति होती है, व्यक्ति को शान्ति एवं आनन्द से आपूरित कर देने की क्षमता होती है। दिव्य नाम में ऐसी अद्भुत रहस्यमयी शक्ति निहित है कि इसका गायन हृदय को पवित्र करके कीर्तनकर्ता को प्रभु-चेतना से सम्पन्न कर देता है।
**✿❀✤❀✿**