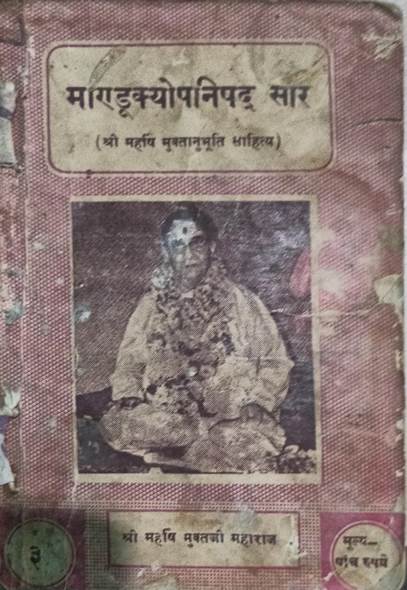
माण्डूक्योपनिषद् सार
(श्री महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य)
प्रकाशक
श्री महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति
केन्द्र, दुर्ग (म. प्र.)
श्री महषि मुक्तानुभति प्रकाशन (३) मूल्य- पांच रुपये
संकलनकर्त्ता-
गिरधारीलाल श्रीवास्तव
स्टेनोग्राफर
सैन्चुरी सीमेंट नेवरा
जिला- रायपुर (म.प्र.)
- प्रकाशक
श्री महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति केन्द्र, दुर्ग (म. प्र.)
卐
(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)
प्रथम संस्करण १००० प्रति चैत्र रामनवमी सन् १९७७ ई०
मुद्रक-
ऋतुराज प्रेस, इन्दिरा मार्केट, दुर्ग (म. प्र.)
दो शब्द
भगवत् प्रेमियो ! मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ विभाग के रायपुर नगर में पुरानी बस्ती स्थित श्रीमहामाया मंदिर के विशाल प्रांगण में श्री सद्गुरुदेव महर्षि मुक्त जी महाराज के श्री मुख द्वारा, सोमवार दिनांक १२ नवम्बर सन् ११७३ से रविवार दिनाक १२ नवम्बर सन् १९७३ तक 'माण्डूक्योपनिषद्' पर आध्यात्मिक प्रवचन हुआ । उसे गुरुनैष्ठिक बन्धु श्री गिरधारीलाल जी श्रीवास्तव (स्टेनो- ग्राफर) सेन्चुरी सीमेंट, नेवरा ने लगातार उपस्थित रहकर पूरा का पूरा प्रवचन शार्टहैण्ड के द्वारा स्वयं तथा जन कल्याण की भावना से लिपिबद्ध किया । इसके उपरान्त बड़े परिश्रम से उन्हें हिन्दी में लिखकर समिति को प्रकाशनार्थ सर्पित किया । इस पुस्तक के प्रकाशन में श्री झुम्मकलाल जी 'दीन, 'सचिव', मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति दुर्ग ने तन मन से अपना सहयोग दिया जिसके फलस्वरूप यह पुस्तकाकार हो, आपके पास तक पहुंच सका ।
मुक्तानुभूति साहित्य प्रकाशन में श्री गिरधारीलाल जी श्रीवास्तव एवं श्री 'दीन जो' द्वारा दिये गये इस सहयोग के लिये समिति उनका बहुत बहुत आभारी है ।
परमानन्द शरस्त्री
अध्यक्ष
मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति, दुर्ग
समर्पण
गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री, गुरवे नमः ।।
परम-पूज्य श्री सदगुरुदेव
महर्षि मुक्त जी महाराज
के श्री चरणों में
सप्रेम सादर
समर्पित

विनीत
गिरधारीलाल श्रीवास्तव
विषय-सूची
(श्री मषि मुक्तानुभूति)
卐 श्री गणेश य नमः 卐
।। श्री गुरवे नमः ।।
प्रथम दिवस का प्रवचन
(सोमवार दिनांक १२ नवम्बर सन् ७३ के १० बजे से दोपहर १२ बजे दिन तक का है।)
…….वन्दना………
(नारायणोपनिषद्)
ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति । नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायु- ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी । नारायणाद् ब्रम्हा जायते । नारायणाद् रुद्रो जायते । नारायणाद् इन्द्रो जायते । नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते ।
नारायणाद् द्वादशाऽऽदित्याः सर्वे रुद्राः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणिच्छदाँसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते ।
अथ नित्यो नारायणः । ब्रह्मा नारायणः । शिवश्च नारायणः । शक्रश्च नारायणः । कालश्च नारायणः । दिशश्च नारायणः । विदिशश्च नारायणः । ऊर्ध्वं च नारायणः । अधश्च नारायणः । अन्तर्बहिश्च नारायणः
नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलको निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् । य एवं वेद, स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ।। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ।।
रामाय राम भद्राय, रामचन्द्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय, सीतायाः पतये नमः ।।
यन्मायावशर्वात विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा ।
यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेभ्रमः ।।
यत्पादप्लव मेक मेव हि भवाम्भो धेस्ति तीर्षावताम् ।
वन्देऽहं तमशेष कारण परं रामाख्य मीश हरिम् ।।
अनन्त नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्वेन प्रस्फुरित, महा- महिम्, स्वआत्मस्वरूप सकल चराचर एवं आत्मजिज्ञासु गण ! उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत ।
अनादि काल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवो ! उठो ! स्व-स्वरूप भगवान आत्मा में जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर अपना आत्मकल्याण करो । मानव जीवन का यही चरम लक्ष्य है । यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवचन श्री माण्डूक्योपनिषद् के आधार पर हो रहा है।
आत्म जिज्ञासुओ !
इसमें सिर्फ बारह मंत्र है, परन्तु सबसे महत्वशाली उपनिषद् माना जाता है और इसकी विस्तृत व्याख्या होती है। अथर्व वेद की ब्राह्मण शाखा से यह उपनिषद् निकली है। वेद चार हैं। और चार उपवेद हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसमें युद्ध कला है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। वेद के दो भाग हैं। एक मंत्र भाग और एक ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण भाग को उपनिषद् कहते हैं उपनिषद् के जितने मंत्र हैं सब वैदिक ऋचाएं हैं।
सनातन ब्रह्म के पास जो पहुंचा दे उसे उपनिषद् कहते हैं ।
उप निषादयति संसारस्य मूल कारण भविद्याम् ।
शिथिलयति ब्रह्म च गमयति इत्युपनिषद् ॥
जो संसार का नाश करे, जो संसार का मूल कारण जो अविद्या है, उसको शिथिल करे और सनातन ब्रह्म जो आत्मा है उसे प्राप्त करादे, उसे उपनिषद् कहते हैं। और ये वेद हैं क्योंकि वेद तो किसी ने बनाया नहीं, ये अपौरुषेय हैं। न ब्रह्मा ने इसे बनाया। ब्रह्मा के चारों मुख से वेद निकले हैं फिर भी ब्रम्हा जी इसके बनाने वाले नहीं हैं।
सृष्टि के आदि में ब्रम्हा जी जब समाधिस्थ थे तो ब्रम्हा जी अपने हृदय में चारों वेदों को सुने, इसलिए वेदों का नाम पड़ा श्रुति । इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। बाद में उसे अपने मुख से प्रकट किए । और शास्त्र को कहते हैं स्मृति ।
ऋषि लोग पर्वतों की कन्दराओं में सैकड़ों वर्ष समाधिस्थ रहते थे । वहां उन्हें पूर्वापर की बातें याद आ गई। स्मरण करके, जो लिखी जाय उसे स्मृति कहते हैं। वेदान्त सिर्फ इतना ही है, उपनिषद् भर । परन्तु जितने भी ग्रंथ हैं, वे श्रुतियों के विरुद्ध नहीं, चलते । श्रुति को लेकर स्मृत्तियां चलती है। और ये कहना चाहिए कि जितनी स्मृतियां हैं वे सब श्रुति की व्याख्या हैं। ये भी नियम स्त अ अ है कि जो श्रुति विरुद्ध सिद्धान्त है वो अमान्य होता है। सार्वभौम वि नहीं होता तो भैय्या ! यह है माण्डूक्योपनिषद् इसका पहला मंत्र है-
ओमित्येत दक्षरमिद्ꣲ᳭ सर्व तस्योप व्याख्यानं भूतं भवभ्दविदिति
सर्वमोङ कार एव यच्चान्यत्त्रिकाला तीतं तदप्योङकार एव ॥१॥
पहले ही घोंट दिया । ओम इति अक्षम् । इदम् नाट्यं जगत । ये सब ओम आत्मा है। ओम् के माने होते हैं 'मैं' । सर्व 'मैं' हूं। अक्षर देखो - अक्षर कहा है, अक्षर कहते हैं जिसका कभी नाश न हो। और जो अक्षर होता है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता । जैसे तुम लिखते हो "क" ।
'क', 'ख', 'ग', 'प' ये सब अक्षर हैं। यदि 'क' का वास्तव में यही आकार है तो जितनी भाषाएं हैं संसार में 'क' ऐसे ही लिखना चाहिए । ये तो हमारे तुम्हारे दिमाग का फुजला है। 'क' जैसा है वैसा ही है। और न लिखने पढ़ने लायक है इसलिय अक्षर कहते हैं। जिस तरह सनातन ब्रम्ह अवांग मनसगोचर है। परन्तु हम अपनी कल्पना करते हैं कि भगवान इस तरह का है, भगवान का ये आकार प्रकार है, आराधना जगत में, जिस प्रकार हम कल्पना करते हैं यद्यपि आकार प्रकार नहीं है उसका, उसी प्रकार हम अक्षर में 'क' वर्गादिक की कल्पना करते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है।
फिर देखो 'क', 'ख' जिस आधार पर 'क' वर्गादिक अध्यस्त है। जैसे लकड़ी आधार है और 'डण्डा' अध्यस्त है। 'सोना' आधार है, 'आभूषण' अध्यस्त है इसी तरह 'क' से 'अ' निकाल ला, अब 'क' कहो तुम ? 'अ' का उच्चारण न हो और 'क' कहक दिखाओ । भगवान ने अपनी विभूति का जो वर्णन किया है- जिसके बिना जिसका उच्चारण ही न हो उसी का नाम 'अक्षर' है। जा अक्षर है ओम् । और जो 'ओम' है वह में हूं इसलिए हमारे यहा भारतीय विज्ञानों की परम्परा है। प्राचीनकाल में विद्वान लोग लेख लिखा करते थे, वे हाथ से लिखे जाते थे । तो हमारे यहा काटने की प्रथा नहीं है कोष्टक बना दे ।
मिट्टी की दिया में हरताल रखते थे, हरताल लेकर उस पर लगा देते थे, तो वो अशुद्धि माना जाता था । ओमिति । 'अक्षरम्' इदम् अपंचम् अक्षरम् जो कुछ भी है, में आत्मा हू, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसकी व्याख्या क्या है ?
आज के पहले जो था और आगे जो कुछ भी रहेगा और अभी जो कुछ है सब ओंकार है। यह 'ओम्' अक्षर की व्याख्या है। सत्, रज, तम तीनों गुणों से जो परे है वह भी ओम है। यानी 'मे' आत्मा हूं। मुझ आत्मा से भिन्न, कुछ भी नहीं । भगवान राम- लक्ष्मण से कहते हैं । अध्यात्म रामायण में-
पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तये-दोड्.कारमात्रं सचराचरं जगत् ।
तवेद वाच्यं प्रणवो हि वाचको, विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ।।
(अ. रामा. उ. का. सर्ग ५ श्लोक ४८ वां)
निर्विकल्प समाधि से प्रथम ऐसा चिन्तन करे । सचराचरम जगत प्रपंचम् ओंकार मात्रम् । सत्ता जगत् प्रपंच 'मैं' आत्मा हूं। ओम् माने 'मैं' प्रणव ब्रह्म सनातन तत्व जो में आत्मा हूं, वह हूं. वाचक और सारा चराचर है वाच्य ।
लकड़ी है 'वाचक', डण्डा है 'वाच्य' । 'सोना' है 'वाचक' 'आभूषण' है वाच्य । 'में' आत्मा 'वाचक' हूं और संसार है 'वाच्य'।
"विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः"
अज्ञानता के कारण ये जगत प्रपंच भास रहा । 'है' नहीं तीन काल में । अज्ञान से ये 'प्रपंच' भास रहा है, 'स्वरूप' देश में नहीं । आत्म जगत में खड़े होकर देखो प्रपंचादिक है ही नहीं । इसका चिंतन समाधि से पूर्व करे ।
पूर्व समाधे …………………..... न बोधतः ।
यदन्यदन्यत्र त्रिभाव्यतेभ्रमा दध्यासमित्याहुरमुं विपश्वितः
असर्पभूतेऽहिविभावनं यथा, रज्ज्वादिके तद्वदणीश्वरे जगत्
(अ. रामा. सर्ग ५ उ. का. श्लो. ३७)
अन्य में जो अन्य का भान, जैसे रज्जू में सर्प का भान; इसको विद्वानों ने 'अध्यास' कहा है। यद्यपि सर्प तीन काल में नहीं है। इसी तरह 'मैं' आत्मा जो हूं उसमें जगत् प्रपंच, रज्जू में सर्प के समान भास रहा है। तो भैय्या एक होता है अध्यास और दूसरा होता है अभिमान । स्वरूप आत्मा 'मैं' में देह जो है, अध्यास है। इसलिए कहते हैं देहाध्यास । है तो रस्सी की रस्सी ही, परन्तु उस रस्सी को हम सर्प देखते हैं, और सर्प मानकर ही हमें भय और कम्पन होता है ।
ऐसे स्वरूप आत्मा में 'देह' का अध्यास । तो रज्जू के बिना ज्ञान हुए, जैसे सर्पाध्यास नहीं जाता, उसी तरह बिना अपने स्वरूप भगवान 'आत्मा' को जाने देहाध्यास नहीं जाता ।
चाहे जितना कर्म करो, जितनी उपासना करो, वेदान्त के ग्रंथों को पढ़ते रहो रात-दिन । जब तक स्वरूप 'आत्मा' का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक देहाध्यास कभी नहीं जाता । आनन्द लो !
जब तक देहाध्यास नहीं जाता तब तक देहाभिमान नहीं । किस तरह जायगा ? कोई-कोई कहते हैं स्वामी जी ! मुझे विषय तो समझ में आ गया है पर देहाभिमान नहीं जाता, तो तुम कहाँ समझे हो तुम्हारी बुद्धि समझी है। अपने राम तो कश्मीर में बैठे हैं।
'ठंडा हो कलेजा जहां, कश्मीर उसे कहते हैं ।'
दो प्रकार की समझ होती है। एक समझ होती है बुद्धिगम्य और एक समझ होती है अहमगम्य । देह नहीं मैं आत्मा हूं इसको 'में' समझता हूं। देह नहीं में आत्मा हूं ये बुद्धिगम्य है। तीन काल में देह है ही नहीं इसे 'मैं' समझता हूं। एक ही वाक्य के अन्दर दो भाव निहित हैं । साहित्यिक है- देह नहीं जन्म-मरण वाला है ये में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसको बुद्धि समझती है। देह नहीं में आत्मा हूँ। देह है ही नहीं तीन काल में, 'मैं' आत्मा ही हूं।
इसको समझकर लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि देहाभिमान नहीं जाता, स्वामी जी ! आनन्दम् ब्रह्म आनन्द ब्रह्म । डूच जाओ इस आनंद सागर में, खो को अपनी वजूद, बहादो सारे अध्यास ।
तो देह नहीं में आत्मा हूं। देह नहीं पांच भौतिक है। ये विनाशशील है। 'शरीर' दृश्य है 'मैं' 'द्रष्टा' हूं। अपने आपको साढ़े तीन हाथ का मानकर अपने को शरीर से भिन्न मानता है। शरीर जन्मता है, मरता है। स्त्री है, पुरुष है, बालक है, युवा है, वृद्ध है। इसको बुद्धि ग्रहण करती है और जिन्दगी इसी में खत्म हो जाती है और देह तीन काल में है ही नहीं, ''मैं'' आत्मा हूं। यहां पर जो साहित्य कहते हैं न, वह सब परे हो जाता है। इसको में ही ग्रहण करता हूं। जिस प्रकार अपने आपको साढ़े तीन हाथ का देह माना वैसे ही अपने आपको बुद्धि भी तो माना । देह नहीं 'मैं' आत्मा हूँ । यदि यह बोध होता है तो बुद्धि गई और बुद्धि से निकलने वाला जो साहित्य है वह भी गया। ये है ठोस वेदान्त, यही ठोस अध्यात्म है ।
अभी तो राम भगवान कह गए-
पूर्व समाधे ……………………………... न बोधतः ।
इसलिए अध्यास को पहले त्याग करो फिर अभिमान तो अपने आप चला ही जायगा । अपने स्वरूप भगवान आत्मा को जान लेने पर अध्यास का त्याग होता है। अध्यास के त्याग पर अभिमान का त्याग हो जाता है। दूसरी चीज यह है कि देहाध्यास के त्याग में स्वरूप ज्ञान । स्वरूप ज्ञान में देहाध्यास का त्याग और देहाध्यास के त्याग में देहाभिमान का त्याग होता है यद्यपि बुद्धि द्वारा समझा है- देह नहीं, आत्मा हूं। यहां पर क्या भान होता है कि आज के पहले 'में' जीव था और अब ब्रम्ह हुआ । आज के पहले बद्ध था अब 'मुक्त' हुआ । आज के पहले मैं 'अज्ञानी' था अब 'ज्ञानी' हुआ। अध्यास तक ही यह धारणा रहती है और अध्यास चले जाने पर
इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्यः स्यन्दन्तेपश्चात्प्रतीच्यस्ता समुद्रात्समुद्र मेवा
पियन्तित्पसमुद्र एव भवतिता यथा तत्र न विदुरि- यमहमस्मीय महमस्मीति ॥१॥
(छांदोग्य उपनिषद)
गंगा, यमुना - कावेरी जितनी छोटी बड़ी नदियाँ हैं संसार की; जब समुद्र में मिलती हैं तो उन्को पूर्वा पर का भान नहीं रहता कि आज के पहले 'मैं' गंगा, यमुना थी और अब में समुद्र हो गई। यह। याद कौन करे !
मुक्ता जब मिला समंदर से, तब कौन किसी की याद करें।
बस इसी लहर में लहराना कोई क्या समझे, कोई क्या समझे !
और अभी याद है तो मत समझो समुद्र से मिली है। बाहर से चिल्ला रही है, यह श्रुति ही छान्दोग्योपनिषदकी है जब स्वरूप का पूण बोध हो गया तो अध्यास का त्याग और अध्यास के त्याग से अभिमान का त्याग । तब कौन याद करे कि आज से पहले में जीव था या ब्रह्म था। जीव की अपेक्षा से ही तो ब्रह्म भाव था। जब जाव ही चला गया तो ब्रह्म भी चला गया। वेटा मरा तो बाप भी मर गया। इसी तरह पूर्ण रूप से स्वरूप के बोध होने पर यह स्मृति नहीं रहती कि आज के पहले जीव था ।
अब यहाँ एक प्रश्न होता है, कि अधिष्ठान में जो अध्यस्त होता है वह अधिष्ठान के अनुरूप होता है। यह प्रश्न है.? अरे सफेद धागा यदि अधिष्ठान होगा तो वस्त्र भी सफेद होगा। लकड़ी काणी होगी तो डंडा भी काला होगा । रज्जू टेढ़ी-मेढ़ी होगी तो सांप भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। यह निविवाद सिद्धांत है । तो यहाँ प्रश्न होता है कि जैसे कि यह देह दिखाई दे रहा है ? अरे मुझ आत्मा में "भास रहा है तो क्या में भी इसी तरह आकार-प्रकार वाला हूँ? यह पूर्व-पक्षी की शंका है ! अधिष्ठान में जो अध्यस्त भासता है वह अधिष्ठान हो तो है। अधिष्ठान का नाम अध्यस्त कव पड़ता है ? जैसा है उसको वैसा न जानकर कुछ का कुछ मान लेना अध्यस्त है। रज्जू अधिष्ठान है सर्प अध्यस्त है जैसा अधिष्ठान रज्जू है वैसे ही उसको न जानकर उस रज्जू को सर्प मान लेना अध्यस्त है। अन्य में अन्य का भान होना. इसका नाम है अध्यास । तो फिर अध्यास भी तो अधिष्ठान का ही अज्ञान कहा जाता है। रज्जू के अज्ञान से ही तो हम रज्जू को सर्प कहेंगे । अध्यास के अस्तित्व में हो तो अधिष्ठान कहा जायगा । अध्यास के अभाव में अधिष्ठान का भी तो अभाव है। तो देह हुआ अध्यास और 'मे' हुआ उसका अधिष्ठान । जिस तरह रज्जू को सर्प मानने में हुआ । रज्जू में अध्यस्त अथवा अध्यास । इसी तरह स्वरूप आत्मा को साढ़े तीन हाथ का मान लेना अध्यास अथवा अध्यस्त है।
अब यहां शंका होती है ? कि जब अधिष्ठान के अनुरूप ही अध्यस्त होता है। तो क्या इसी तरह में अधिष्ठान आत्मा हूं ? यह शंका है। जी नहीं अरे ! 'में' आत्मा को जब देह मानोगे तब न आकार प्रकार का विकल्प होगा और जब अपने 'मैं' आत्मा को 'में' ही जानोगे, कुछ न मानोगे तो फिर देह नहीं । देह नहीं तो देह का आकार-प्रकार नहीं । अरे, अध्यास को मानकर ही तो ये विकल्प उठा, कि क्या में ऐसा हूं ?
'मैं' भगवान आत्मा ज्ञान पुञ्ज हूँ। ज्ञान सागर हूं, ज्ञान निधि हूं। कोई अनुभूतियाँ तो नहीं हैं। असीमित है। अपार है। देहा- दिक प्रप्रंच, तृण से आदि ब्रह्मा तक सारा चराचर मुझ आत्मा में अध्यस्त है। मानना अध्यास, देखना अध्यस्त है। रज्जू को सर्प मानना अध्यास है, रज्जू को सर्प देखना अध्यस्त है। अधिष्ठान एक ही रहेगा तो पृथ्वी ऐसी है, वायु ऐसा है, आकाश ऐसा है। पंच महाभूतों के विभिन्न-विभिन्न प्रकार के रूप और रंगों का विकल्प और फिर पंच महाभूत से निकले हुए पंच विषय । रज्जू से भय कंपन होता है, कि सर्प से भय कंपन होता है ? सर्प से भय और कंपन होता है गोया विकल्प से भय और कंपन होता है न कि रज्जू से । तो में आत्मा में जब देहादिक प्रपंच का विकल्प हुआ तभी आकार- प्रकार का विकल्प होता है।
अपने आप, 'मैं' को, साढ़े तीन हाथ का देह मानना या तो साढ़े तीन हाथ को स्वरूप मानना, और इसको साफ करेंगे । अपने 'मैं' आत्मा को जगत प्रपंच मानना, देहादिक प्रपंच मानना यह ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। और 'मैं' ही तो हूं जिसे देह मानते हो यह ज्ञान है। 'मैं' को जानकर 'मैं' देह हूं ऐसा कहना यह अज्ञान है। काल्पनिक जगत में तो कहेंगे ही। बाली को बाली कहेंगे, हार को हार कहेंगे, चैन को चैन कहेंगे । काल्पनिक जगत में तो कहना पड़ता है। मगर दृष्टि वही स्वर्णाकार होगी। मगर काल्पनिक जगत में तो देह कहेगा न । मगर इस कथन में कोई सत्यता नहीं है। आगे चलो। क्यों जी ? सब कुछ 'में' आत्मा हूं, मुझ 'आत्मा' से भिन्न कुछ भी नहीं तो अगर कोई कहता है कि 'में' देह हूं, तो क्या बुरा है। स्वरूप देश में ज्ञान-अज्ञान की कल्पना है कि स्वरूप से बाहर ? जिस तरीके से सूर्य में न अंधकार है न प्रकाश । उसी प्रकार मुझ आत्मा में न ज्ञान है न अज्ञान । यह ज्ञान है, यह अज्ञान है। यह भी तो मुझ आत्मा पर अध्यास है। इसका विकल्प भी तो बुद्धि ने ही किया है। भैय्या ! अगर बुद्धि से समझ रहे हो तो फिर कल्पना उठेगी और स्वयं समझ रहे हो तो ! ये जो उपनिषद् है, वह खुद के समझने वाली है। बुद्धि की चीज नहीं है। 'मैं' ही हूं और में' हूं। अध्यास हटाने के लिए 'में' ही हूं और अध्यास हट जाने पर "मैं' हैं। रज्जू ही है। सर्पाध्यास हट जाने पर तो नहीं कहा जाता कि रज्जू ही है। रज्जू ही है कहने से पता लगता है कोई चीज और है। जब अध्यास हट गया तो मैं हूं। प्रपंच दरिद्र है। देव उठनी एकादशी के दिन औरतें गन्ने के टुकड़ों से सूपा पीटतो हैं। दरिद्र को पीट-पीट के घर से बाहर निकालती हैं। प्रपंच रूपी दरिद्रग्को हृदय रूपी घर से निकालने के लिए हम दस बजे से सूरा पोट रहे हैं। जब दरिद्र निकल जाता है तो अटूट खजाना तो है हो ।
समय २ बजे से ४ बजे तक
ओम का अर्थ होता है 'में' । तृण से लेकर ब्रम्हा पर्यंत सारा चराबर में 'आत्मा' हूँ । मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। तो इसकी व्याख्या क्या है ? जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होगा या रहेगा मुझ से भिन्न कुछ भी नहीं यह इसको व्याख्या है।
देखो ! उस वक्त कहा गया था अध्यात्म रामायण का जो श्लोक भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा है उसमे थोड़ा सा रह गया है बताने को ।
पूर्वम् समाधे .... ……………….. सचराचरम् जगत् ।
निर्विकल्प समाधि से पहले इस प्रकार का चितन करे- जो कुछ भी है, सारा जगत प्रपंच ओम् 'मे' आत्मा हू। क्योंकि कहते - हैं कि अपने स्वरूप आत्मा के अज्ञान से सारा प्रपच भास रहा है, दिखाई दे रहा है, अज्ञान के कारण । स्वरूप देश से नहीं, आत्म देश से नहीं। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि समाधि से पहले इस प्रकार का चितन क्यों करे ?
यह मसला उस वक्त हल नहीं हुआ था। समाधि कहते किसको हैं? चित्त वृत्ति निरोधः समाधिः ।' चित्त की स्थिरता को कहते हैं-- समाधि । चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त की स्थिरता के लिए यह परम साधन है कि मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है । समाधि की सिद्धि का यह परम साधन है कि, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। क्यो ? चित्त जो है, यह मन जो है दौड़-दौड़कर विषय में जाता है। शब्द में स्पर्श में, रूप में, रस में गध में । चित्त का दृश्य जो है वह विषय है। 'अहमेद सर्वम्' मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, 'मैं' ही हू तो यह जांयगा कहां?
"देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि ।
यत्र-यत्त्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः ।।''
जहां-जहां मन जाता है वहां-वह समाधियां हैं। मन शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि में जाता है। जिसको यह मन विषय समझ- कर जाता है वह जब मुझ आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं तो यह मन जायेगा कहाँ ? यह मन समाधिस्थ हो जाता है। निरोध का मतलब और होता है। निरोध का नाम है रोकना। जैसे नदी का रुकना और नदी का स्थिर हो जाना। बांध डाल दो, नदी रुक जाती है। स्थिर करने के लिए कोई साधन नहीं है। नदी का जो स्वाभाविक बहाव है वह जंगल, पहाड़ की ओर नहीं है। नदी का स्वाभाविक बहाव समुद्र की ओर है। नदी को स्थिर करने के लिए कोई बांध डालने की जरूरत नहीं है। नदी तो समुद्र में ही जाकर स्थिर होगी । इसी तरह मन एक नदी के मानिन्द है ।
चित्त को निरोध करने का साधन तो है स्थिर करने का कोई साधन नहीं है। अब चित्त को स्थिर करना है। जब मुझ आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है तो फिर यह जायेगा ही कहां ? अरे ! जब- सब कुछ 'मैं' ही हूं। तो आने-जाने वाला यह चित्त कौन है ? यह भी तो 'मैं' ही हूं। जाएगा कहां ? शान्त हो जायेगा ।
उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादजं सर्वमुदाहृतम् ।
न च भूतादभूतस्य संमवोऽस्ति कथंचन ।
(गौ. पा. कारि. अलात् शांति प्रकरण मं. क्र. ॥३८॥ )
जगत् प्रपंच का जो उत्पादन है उसकी अप्रसिद्धि है। विश्व 'में किसी की ताकत नहीं है कि प्रपंच को सिद्ध करके बता दे । उत्पादन की अप्रसिद्धि के कारण यह सारा प्रपंच अजन्मा है। इसका जन्म ही नहीं हुआ । क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं होती ।
"स्वतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते ।
सदसत्सदसद्वापि न किंचिद्वस्तु जायते ॥ २२ ॥
(गौ. पा. कारि. अलात्शान्ति प्रकरण मंत्र क्र. ॥२२॥)
यह संसार न तो स्वयं पैदा हुआ है न इसे किसी ने पैदा किया है। यदि कहो संसार जंजाल पैदा होता है। तो यह पैदा होने के पहले भाव रूप था कि अभाव रूप था । न इस देह को किसी ने पंदा किया न यह देह स्वयं पैदा हुआ । यदि मानो कि पैदा हुआ हैं तो पैदा होने के पहले क्या था ? सत्य था कि असत्य था ? तो सत्य मानकर भी पैदा होना सिद्ध नहीं होता और कहो असत्य रूप था- तो जो है ही नहीं वह पैदा क्या होगा ? इसलिए संसार प्रपंच की जो उत्पत्ति है वह सिद्ध नहीं होती । इसलिए इदं प्रपचं अजम् । 'अजम्'- जन्म हुआ ही नहीं अजत्वादऽहम् और अजन्मा होने से. 'में' हूं।
“भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि ।
अभूतस्यापरे धोरा विवदन्तः परस्परम् ।।''
(गौ. पा. कारिका अलात् शान्ति प्र. मं. क्र. ।॥३॥)
संसार की उत्पत्ति मानकर ही आपस में लोग विवाद करते हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ बतलाता है। परन्तु ऐसा नहीं है। शरीरादिक प्रपंच हुए ही नहीं तीन काल में, सब वैतथ्य है।
तथ्य कहते हैं, वास्तविकता को । वास्तविकता जिसमें न हो उसे 'वैतथ्य' कहते हैं । जो आदि में न हो और अंत में न हो और मध्य में यह कहां से पैदा हो गया ? अरे ! यह भी नहीं है। देखने से मालूम होता है कि- 'है' । 'है' के सदृश मालूम होता है, 'है' नहीं मालूम होता है। पहले भी सर्प नहीं है। अंधकार में जो सर्प दिखाई देता है वह पहले भी नहीं है, अन्त में भी नहीं है। बीच में दिखाई देता है वह भी तो नहीं है - ररसी ही है। उजाले में यदि उसी स्थान में सर्प दिखाई दे तब समझो कि अंधकार में जो दिखाई दे रहा है वह सर्प है। 'वैतथ्य' है। वास्तविकता से हीन है, है ही नहीं तीन काल में ।
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।
वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ।।३१॥
(गोंड़ पा. कारि. अलात् शान्ति. प्र. प्र. मंत्र क्र. ।३१।।)
पहले भी यह प्रपंच नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा तो फिर बीच में यह ससार कहां से आ गया। पहले था तो 'में ही था और आखिर में जो कुछ रहेगा तो 'मैं' ही रहूंगा। यह बीच में कहां से आ गया प्रपंच ? निकालो दरिद्र, पीट-पीट के जिसको तुम संसार मानते हो, प्रपंच मानते हो, यह भी नहीं है क्योंकि ''अजम्'- 'में' ही हूं । सनातन तत्व है। जब मुझ 'आत्मा' से भिन्न कुछ नहीं तो यह निश्चय होने पर क्या होता है 'देहाध्यास' चला गया और अध्यास के चले जाने पर उसका अभिमान था वह भी चला गया । अब रह गया विशुद्ध तत्व 'आत्मा' का 'आत्मा' । अरे! यही तो समाधि है। इसी का नाम तो निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि तो चित्त की होती है और एक निर्विकल्प समाधि मुझ निर्विकल्प आत्मा की होती है। जो चित्त की निर्विकल्प समाधि है वह, साधन का फल है और मुझ निर्विकल्प आत्मा की 'जो समाधि है वह आत्म तत्व के बोध का फल है। तो जो चित्त के निर्विकल्प की समाधि है वह एन-केन-प्रकारेण चित्त किसी साधन द्वारा रोका जाता है लेकिन वह समाधि क्षणिक होती है। चन्द घंटे के लिए हो, चन्द दिनों के लिए हो, चन्द कल्प के लिए हो। वह कभी न कभी टूटती ही है। और वित्त के निर्विकल्प की जो समाधि है वह परदेश की है, स्वदेश की नहीं है क्योंकि चित्त को निर्विकल्पा करने का जो विकल्प है, चित्त हमारा निर्विकल्प हो, चित्त हमारा निरोध हो यह तो जीव देश में होता है, न कि आत्म देश में । यह जो वस्तु लखाई जा रही है वह स्वदेश की चीज है अष्टांग योग करके जो साधन द्वारा समाधि लगाई जाती है वह 'इनडायरेक्ट' (Indirect) है । और अभी जो बताई जा रही है वह 'डायरेक्ट' (Direct) है। जब मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं तो चित्त 'मैं' ही हूं। इन्द्रियां 'मैं' ही हूं। 'ओमित्येदक्षरम्' है तो समाधि ही समाधि है ।
किसी-किसी हृदय में विकल्प होता है कि अगर हम समाधि में है तो आवाज हमारे कान में क्यों सुनाई देती है। अरे ! यार- जो पंहित के पत्रा में वह पंडिताइन के अंगुली में । अगर हम समाधिस्थ हैं तो कान में आवाज नहीं आनी चाहिए अगर यह अनुभव करते हो तो सच्चाई से दूर हो । जब 'ओमित्येदक्षर सर्व' तो आवाज भी अध्यास है। अगर मानो तो आवाज है और न मानो तो 'मैं' ही हूं।
"अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते ।
वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निःसङ्.गं विनिवर्तते ॥७९॥
(गौड पा. कारि. अलात् शांति प्रक. मंत्र क्र. ।।७९।।)
जो अभूत है, मन जो है ही नहीं तीन काल में उसमे इस चित्त का 'अभिनिवेश' है। 'अभिनिवेश' कहते है 'आग्रह' को जो 'अमृत' है वह वैतथ्य' है। उसको यह चित्त 'है' ऐसा मानकर जाता है। मगर जब वहां जाता है तो वस्तु का अभाव देखता है, तो स्वरूप में वापस आ जाता है। अभूत में इस चित्त का आग्रह होता है जैसे मृगजल है नहीं, केवल जलाभास है क्योंकि हरिण मानता है कि जल है और छलांग मारकर जाता है और जल नहीं पाता तो निस्संग हो जाता है। वस्तु के अभाव से निस्सग हो जाता है याने यह मन निविषय हो जाता है। मन का निस्संग होना याने मन का ब्रम्ह हो जाना । 'मैं' आत्मा हो जाता है। स्वरूप ही हो जाता है, यह 'मन' । तो वस्तु का अभाव जानकर याने जल का अभाव जानकर वह हरिण लौट आता है, निराश हो जाता है। यही निस्संगता है। निविषय हो जाता है।
"अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निविषयं मनः ।
स्नानं मनोमल त्यागः शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।।"
"श्रुति"
अभेद दर्शन-मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है यही तो ज्ञान है और मन निविषय हो जाता है, यही ध्यान है। आंख बन्द करने के मायने ध्यान नहीं है। आंख बन्द हो जाय मगर मनीराम बन्द हो जाय तब न । मन निविषय हुआ तो मन कहाँ रहा, भग- वान हो गया स्वरूप ही हो गया।
अभेद दर्शनं ज्ञानम्; ध्यानं निविषयँ मनः ।
'मन' का मल है विक्षेप । खामख्वाह जो चीज नहीं है उसको मान रहा है यह अनादिकाल से ।
"स्नानं मनोमल …………... शौचमिन्द्रिय निग्रह ॥"
जैसे रज्जू में सर्प की भ्रांति होती है ऐसे ही सर्व में व्यापक जो 'मैं' सनातन ब्रम्ह हूं तृण से आदि ब्रम्हा पर्यंत सारे चराचर का जो कल्पित ज्ञान यह अज्ञान है। अभेद दर्शन क्या है ? याने इसका क्या प्रमाण है कि मुझ आत्मा का, अपने आपको अपने स्वरूप आत्मा का ज्ञान है क्या ? इसका क्या प्रमाण है ? इसका प्रमाण यह है कि अपने स्वरूप 'मैं' आत्मा से एक तिनके से लेकर ब्रम्हा पर्यंत कोई भी भिन्न न दिखाई दे। अपने से किसी की जुदाई दिखाई न दे कि में ज्ञानी हूं और तुम अज्ञानी हो। यह प्रमाण है। यह मीटर है। अपने से दूसरे की प्रतीत न हो इसी का नाम अभेद दर्शन है, भेद न देखना ही अभेद दर्शन हैं ।
'ब्राम्हणे पुल्कसे स्तेने ब्रम्हण्येऽर्के स्फुलिगके ।
अक्रूरे क्रूर के चैव समदृक् पण्डितोमतः ।।''
(श्रीमदभागवत् एका. स्कंघ, अध्याय २९ श्लोक १४)
अक्रूर और क्रूर में जब भेद दिखाई न दे वह ब्राम्हण है ।
'विद्या विनय सम्पन्ने ब्राम्हणेगविहस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समर्दाशनः ॥
(श्रीमद्भग. गीता अ. ५ श्लो. १८)
अभेद दर्शन किसकी देन है ?
ओमित्येदक्षरमिद सर्वभ्- इसकी देन है। जब मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं तो भेद दृष्टि का स्वभावतः त्याग हो जायेगा। रामायण की चौपाई कहती है।
'ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं, देखत ब्रम्ह रूप सब माहीं ।
जहां एकउ नाहीं मान तहँ ज्ञान और जहां ज्ञान- देखत ब्रम्ह रूप सब माहीं । यही अभेद दर्शन है। किसी किस्म की मान्यता न हो न ज्ञान की न अज्ञान की, न बद्ध की न मुक्त की। यह नारा- यण पद का बोध कराया जा रहा है न कि ज्ञान पद का। यह नारायण पद का विवेचन है। तो क्यों भैय्या ? भगवान देश में भी 'मैं' ज्ञानी हू । क्या भगवान भी मानता है कि मुझे स्वरूप का बोध हो गया, तुम्हें नहीं हुआ। उस देश का परिचय तुम्हें दिया जा रहा है, उस देश का दर्शन तुम्हें कराया जा रहा है। यह भगवान पद है यह नारायण पद है। यहां न जीवभाव है न ब्रम्हभाव है न ज्ञानी भाव है न अज्ञानी भाव है और यदि भाव है तब सब चीजों का भाव एक है। 'ओमित्येदक्षरमिदं सर्वम्' एक प्रश्न होता है ?
स्वामीजी, जब मुझ आत्मा से भिन्न कोई है ही नहीं तो फिर यह पुण्यात्मा और पापी, ऊंच-नीच, ज्ञानी-अज्ञानी और फलां धर्म, फलां मजहब और फलां सोसायटी यह क्या है ?
अरे यार इसी का नाम तो "अज्ञान" है। यहाँ तो ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है स्वरूप देश में खड़े होकर तुम प्रश्न करो तो इसका उत्तर सोचा जाय । मन का निविषय होना क्या है ? चाहे मन के निविषय होने का नाम ध्यान कहो, अथवा मन के आत्मा हो जाने को, सनात्तन ब्रम्ह हो जाने का नाम ध्यान कहो एक हीं बात है ।' क्योंकि आत्मा निविषय है। तो मन जब निविषय हो जाता है, निविषय हो जाना याने स्वरूप हो जाना ।' संकल्प और विकल्प से जो यह मन रहित हुआ तो आत्मा हो जाता है यह मन । इसी का नाम है ध्यान । यदि यह विकल्प होता है कि अभी स्वामी जी ने थोड़ी देर के लिए अनम्यास के अभ्यास में बैठाया था तो आवाज क्यों आई ? तो बेहोशी को समाधि कहते हैं तो इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है ? क्लोरोफार्म सूंघ लो, नींद की गोली खातो फिर तुम्हारे ऊपर चाहे अजगर चढ़े समाधि ही समाधि है। अरे समाधि तो उसे कहते हैं कि जिस अवस्था में तुम्हारी 'घी' याने बुद्धि सम हो जाय, उसको समाधि कहते हैं। इस हो खूत्र बताएँगे।
यह देह है। देह को जानने पर देह है कि देह को मानने पर देह है ? देह को मानने पर देह है जानने पर तो 'में' आत्मा ही हूँ। इसी तरह आवाज को जानने पर आवाज है कि आवाज को मानने पर आवाज है तो फिर मानते ही क्यों हो ? देखो, किस समय आवाज, आवाज नहीं है, आवाज 'मैं' हूँ। जब यह विकल्प न उठे कि यह आवाज है।' आवाज सुनने से चित्त को जब ग्लानि न हो तब समझना आवाज 'मैं' हूँ। कान में आवाज आने से 'अरे' ऐसा न हो शोक न हो ।' आवाज न आए तो हर्ष न होय तव समझना कि 'में' हूँ। तब समझना कि यह मन निविषय हो गया । शब्दा- दिक विषय के ग्रहण त्याग में मन जब उदासीन हो जाय तब समझना यही निविषय मन है और यही भगवान का ध्यान है। और यही मन का निस्संग होना है। मन का निराश होना है। "उदासीन बदासीनम्" और यही भगवान कृष्ण का अनासक्त योग है ।।
'अभूताभिनिवेशाद्धि सदृश .... निःसङ्गं विन्विर्तते ॥७९॥
(वही)
'अभूत' कहते हैं- खामख्वाह किसी को मान लेना । यदि बाई आप के शब्दों पर ध्यान नहीं देता अपना हो मारता है उसे अभि निवेश कहते हैं। अभाव में अभिनिवेश होने से याने आग्रह करने से यह चित्त जाता है ग्रहण करने के लिए मगर जिस वस्तु को ग्रहण करने के लिए यह चित्त जाता है, उसका अभाव जानता है जब अभाव जानता है तो निराश हो जाता है। निर्विषय हो जाता है याने भगवान आत्मा हो जाता है थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं कि एक समाधि होती है चित्त के निर्विकल्प की और एक समाधि होती है निर्विकल्प की। निर्विकल्प माने आत्मा ।
चित्त के निर्विकल्प की समाधि है वह तो लगाई जाती है । अष्टांग योग इसी के लिए है। परन्तु निर्विकल्प की जो समाधि है, स्वरूप की जो समाधि है यह लगाई नहीं जाती यह स्वभावतः सिद्ध है यह पहले से ही है। और इसी निर्विकल्प आत्मा की ही समाधि में सारे काम रात-दिन हो रहे हैं। तो फिर तुम क्या समझा रहे हो ? तुम क्यों सूपा पीट रहे हो ? यही समझा रहे हैं। हम कोई नई चीज़ नहीं समझा रहे हैं। तुमको स्वरूपस्थ कराने के लिए, तुमको स्वरूप ज्ञान कराने के लिए नहीं कह रहे हैं। स्वरूप ज्ञान तो तुम्हें पहले से ही है। स्वामीजी पहले से है ? हाँ जी ! पहले से है। कैसे है ? बताते हैं- "में हूँ" यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला ? "मैं हूँ” कहाँ, किस स्कूल में किस कालेज में किस गुरू से पढ़े ? स्वतः सिद्ध है न । चाहे देह मानकर हूँ। चाहे पशु पक्षी मानकर 'मैं' हूँ। मगर 'में' हूँ यह ज्ञान कहाँ से मिला। और हर हालत में 'मैं' ही तो हूँ। "मैं हूँ" का ज्ञान कहीं से नहीं मिला स्वतः सिद्ध है। "में" का ज्ञान सभी को है। भैय्या ! इसी का नाम तो ज्ञान है। "में" 'हूँ' । क्यों जी जब देह की कोई याद कराता है तब में देखता हूँ ? दूसरे के कहने से । यदि में देह हूँ, यह ज्ञान सत्य है, तो हमारे व्यावहारिक जगत के प्रत्येक कार्य में मुझ आत्मा का देह भाव क्यों नहीं रहता ? यहां न प्रक्रिया है न सिद्धांत है। अभी जैसे कथा सुन रहे हो तो देह भाव में सुन रहे हो कि आत्मभाव में सुन रहे हो ? आत्म भाव में। इसी तरह तुम्हारे जितने कार्य व्यावहारिक जगत में होते हैं वे देह भाव में होते हैं कि आत्म भाव में ? तो यह 'में' का ज्ञान कहाँ आसमान से आया ? स्वतः सिद्ध है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही लखा देते हैं। अरे भाई ! में देह हूँ यह में बोल रहा हूँ कि देह बोल रहा है कि नाक बोलती है कि कान बोलता है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं ? अरे ! जो में हूँ, ऐसा "में" ही कहता हूँ, कि ये इन्द्रियां अथवा शरीरादिक ? 'में' ही कहता हूँ। तो फिर यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला ? इसलिए देह नहीं "में" आत्मा हूँ यह कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अब हो गए न देहादिक प्रपंच वैतथ्य ! ये वंतथ्य है याने तथ्य ही नही है.।
आदावन्ते च यन्नास्ति ……………………………… इवलक्षिताः ॥३१॥
(गौड़ पा० कारि० अलातशान्ति० मंत्र सं ॥३१॥)
आदि अंत में नहीं तो वर्तमान में भी नहीं । सत्य के समान अक्षित तो होता है, पर है नहीं। तो इसी तरह मन न पहले था, न मन अंत में है, न वर्तमान में है। यह मन "वैतथ्य" है याने तथ्यहीन है और इसके अंदर जो तथ्य है वह "में" हूँ। अब जब यह चित्त नहीं तो चित्त कल्पित दृश्य भी नहीं। प्रश्न होता है- कि जब संसार प्रपंच तीन काल में है नहीं तो यह पैदा तो नहीं हुआ "प्रपंच” । इसका कोई वजूद नहीं है देहादिक प्रपंच का । 'है' नहीं, माना जाता है। मन को किसने माना ? मन मुझ आत्मा की सृष्टि है। तभी तो कहता हूँ, मेरा मन । मेरा पुत्र, जो पिता कहता है तो अपने आपको कहता है कि अपने से भिन्न को ? जो जिसकी चीज होगी उसी को तो कहेगा। किसी के पुत्र को उसका पिता ही कह सकता है-- मेरा है। पुत्र वेतथ्य है। पुत्र के अन्दर जो तथ्य है यह पिता का है ।
मुझ आत्मा पर मन का अध्यास है। परन्तु एक चीज और समझो । 'मैं' तथ्य रूप 'आत्मा' को ही वैतथ्य मन ने जगत प्रपंच माना है। तो मन का भी अधिष्ठान और प्रपंच का भी अधिष्ठान में ही हूँ। 'मं' हो तथ्य हूँ और बाकी सब वतथ्य है। इसीलिए-
"चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभास तथैवच !
अभूतो हि यतश्चार्थों नार्थाभासस्ततः पृथक"
(गौ० पा० कारि० आमातशा० प्र० मं० सं० ।।२६।।)
न तो यह चित्त पैदा होता है न यह चित्त जिसमें जाता है वह दृश्य पैदा होता है। तो चित्त और दृश्य दोनों की जो उत्पत्ति मानते हो, इनको मानना ऐसा है कि जैसे आकाश में पक्षी के चरण चिन्ह देखना है। चित्त कहो, मन कहो, देह कहो । इसी तरह संसार प्रपंच की उत्पत्ति मानना ऐसे ही है जैसे आकाश मण्डल में पक्षी के चरण चिन्ह देखना ।
अब चार बज रहे हैं, आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है।
ॐ पूर्ण मदः पूर्ण मिदं, पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण मेवाव शिष्यते ।।
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! ! शान्तिः !!!
द्वितीय दिवस का प्रवचन
(मंगलवार दिनांक १३ नवम्बर सन् १९७३ समय १० से १२)
कल के प्रसंग में पहले मंत्र की व्याख्या हुई थी।
ओमित्येतदक्षर मिदꣲ᳭ सर्व तदप्योङकार एव !
समस्त चराचर "मैं" आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इसकी व्याख्या क्या है ? तो कहते है-- जो था, जो है, जो रहेगा सब कुछ 'मैं' आत्मा हूँ।
जिज्ञासुओ !
"नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन ।
न पृथङ नापृर्थाक्कचिदिति तत्त्वविदो विदुः ॥
(गो० पा० कारि० वैतथ्य प्रकरण मत्र सं० ॥३४॥)
न तो आत्मभाव से नानात्व है और न स्वयं अपने भाव से नानात्व है। न स्वयं करके यह अनेक है यह जगत प्रपंच । न अपने करके नाना है यह जगत प्रपंच । माने एक है। न यह किसी से भिन्न है, न किसी से अभिन्न है। जब कि अपने आपके सिवाय दूसरी सत्ता है हो नहीं तो फिर पृथक और अपृथक का सवाल ही पैदा नहीं होता । ये जितने श्लोक कहे जा रहे हैं न, ये सब कारिकाए हैं। भगवान गौङपादाचार्य की । भगवान् जगत् गुरू शंकराचार्य के दादा गुरु हुए हैं भगवान गोविन्द पादाचार्य । भगवान गोविन्द पादाचार्य के गुरु हुए हैं स्वामी शुकदेव जी महाराज । ये कारिकाएँ प्रमाणित हैं और वेदान्त के शास्त्री खण्ड में पढ़ाई जाती हैं। बड़े- बड़े जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष हैं, आत्म वेत्ता पुरुष हैं वे ऐसा कहते हैं-- वे ऐसा जानते हैं। अज्ञानी; क्या जानेगा । अज्ञानियों की दृष्टि में तो अनेकत्व ही है।
देखो - यदि अधिष्ठान अनेक हो तो उसमे जो कल्पित पदार्थ है वह भी अनेक हो। जब अधिष्ठान एक है तो उसमें जो कल्पित वस्तु है वह भी एक है। तो जगत प्रपंच का अधिष्ठान 'में' आत्मा हूँ। और मुझ आत्मा में ही जगत जाल अध्यस्त है। आत्म भाव करके यह जो प्रपंच है न तो नाना है और न अपने आप करके अनेक है न नाना है। भिन्न हैं न अभिन्न है। जब अनेक नहीं तो न यह अपने आप से भिन्ना भिन्न का विकल्प तो तब होता हैं जब अपने आप से कोई परे हो । मुझ आत्मा से भिन्न कोई चीज़ और है ही नहीं तो यह प्रश्न पैदा हो नहीं होता । अब इसको तर्क और युक्ति द्वारा समझो :--
जो नाना भाव है याने अनेकता है। यदि अनेकता अनेक में हो तब तो अनेकता अनेक है और यदि अनेकता एक में है तो फिर अनेकता अनेक न होकर एक है। अनेकता का आधार यदि अनेक है तब अनेकता अनेक है और यदि अनेकता का आधार एक है तो अनेकता एक है। अनेकता को यदि अनेक सिद्ध करता है तब तो अनेकता अनेक है और यदि अनेकत्ता की सिद्धि एक में है तो अने- कता एक है। अव प्रश्न होता है ? यहाँ पर कि- हमें तो अनेकता दिखाई देती है। हमें तो अनेकत्ता प्रतीत हो रही है। में तो अनेक देख रहा हूँ। तो मैं एक कैसे समझू ? ठीक है भैय्या ! तुम जो अनेकता देख रहे हो तो तुम एक होकर अनेक देखते हो कि अनेक होकर अनेक को देखते हो तुम जो अनेक को देखते हो तो एक होकर अनेक को देखते हो कि अनेक होकर अनेक को देखते हो । नहीं, एक होकर अनेक को देखते हो । एक से अनेक को देखते हो तो फिर अनेक कहाँ ? अनेक में से एक निकाल लेने पर यदि अनेक अपने स्थान पर बना रहे तब तो अनेक, अनेक है और एक के निकाल लेने पर यदि अनेक नहीं रहता तो फिर अनेक नहीं है, एक का ही नाम अनेक है ।
न आत्मभाव से नाना है और न स्वयं करके नाना है याने नाना है ही नहीं । यह एकता, यह एकत्व कितना ठोस है। यह एकत्व कितना ठोस घन है कि एक पिन भी नहीं जा सकती इसके अंदर और मन एक, बुद्धि एक, चित्त एक, अहंकार एक, प्राण एक, आंख एक, कान एक । स्वामी जी ! तुम आँख को एक कहते हो । आंख तो दो है, समझो - एक आँख सुने और एक आँख देखे यदि ऐसी बात हो तब तो ऐसा कहने में हर्ज नहीं कि आँख दो हैं। अरे ! जो इस आँख का काम वही उस आँख का काम । इसी तरह कान एक हैं। तो फिर अनेकता कहाँ से आई ? कैसे तुम देख रहे हो ? दूसरी चीज़ यह है। अनेक को जो तुम देखते हो । अरे भाई ! अनेक दिखता नहीं क्योंकि जो कल्पित पदार्थ होता है, अधिष्ठान ही है। अरे भाई ! "डंडा-" लकड़ी देख रहे हो कि डंडा । लकड़ी। आभूषण में जो पीलापन देखते हो वह आभूषण का है या सोने का। सोने का लचीला पन देखते हो वह आभूषण का नहीं है सोने का है। गुरूत्वपना याने वजनपना देखते हो वह भी सोने का ही है फिर आभूषण कहाँ ? यह निविवाद सिद्धांत है कि जो वैकल्पिक पदार्थ है वह नहीं दिखता जैसे 'डण्डा' वैकल्पिक है। लकड़ी पर डण्डे का विकल्प किया गया है वस्तुतः डण्डा है ही नहीं लकड़ी है। वैकल्पिक - पदार्थ देखा नहीं जाता। है, ही नहीं तो दिखेगा क्या ? वह तो - फर्जी होता है, विल्कुल झूठा । अभाव रूप है। डण्डे से लकड़ी = निकाल लेने पर अगर डण्डा दिखाई दे तब तो डण्डा दिख रहा है बौर यदि लकड़ी को निकाल लेने पर डण्डा नहीं दिखाई देता तो लकड़ी ही है। जगत् प्रपंच से अपने को निकाल लेने पर यदि प्रपंच दिखे तब प्रपंच दिख रहा है और यदि आत्म तत्व को निकाल लेने पर प्रपंच नहीं दिखता तो फिर "में" ही हूँ।
जो कल्पित पदार्थ है वह दिखता नहीं । खाली शब्द ही शब्द सुनाई पड़े और देखने चलो तो वह वस्तु न मिले उसे विकल्प कहते हैं। देह नहीं दिखता "मैं" देह नहीं दिख रहा है। यह तो विकल्य है और जो भी चीज़ तुम देखते हो वह सभी विकल्प है। जो भो देखते हो अपने आपको देखते हो चीज को नहीं देखते । तो जगत् प्रपंच सुनने की चीज है क्योकि कल्पित वस्तु है। अरे भाई ! जिस मन की शिकायत करते हो कि मन बड़ा चंचल है तो भाई तुमने मन को कभी देखा है। सुना है कि जो आए-जाए उसे मन कहते हैं। जो चंचल हो और स्थिर हो उसे मन कहते हैं। नहीं तो देखे हो तो बतादो कि 'मन' कैसा है ? गोरा है, कि काला है, लम्बा है कि जौड़ा है। कुछ नहीं । सब विकल्प है मुझ आत्मा के बिना देखे, अगर प्रपंच यदि अपने आप दिखता हो तब तो प्रपंच है और अगर मैं देखता हूँ तब दिखता है तो फिर 'मैं' ही दिखता हूँ, प्रपंच नहीं है। 'प्रपंच' को 'प्रपंच' देखता है कि प्रांच को 'में' देखता हूँ । देहादिक प्रपंच को देह को, देह देखता है कि देह को 'में' देखता हूँ, 'मन' को 'में' देखता हूँ, 'चित्त' को 'में' देखता हूँ, 'अहंकार' को 'मैं' देखता हूँ। तो 'मैं' जो 'देह' को देख रहा हूँ तो फिर देह दिख रहा है कि में दिख रहा हूँ ? अरे ! इन्द्रियाँ कल्पित को ग्रहण करती हैं कि मुझ आत्मा अधिष्ठान को ? कल्पित को ग्रहण करती है। कल्पित को विषय करती हैं इन्द्रियाँ, न कि मुझ आत्मा को । इस- लिए न आत्म भाव करके नाना है न स्वयं करके नाना है यह जो देह दिखाई दे रहा है। यह वेह है। जो दिख रहा है, अरे दिखने वाला देह है या देखने वाला देह है समझो ! याने यह जो देख रहे हो यह दिखाई दे रहा है। तो दिखने वाले को देह कहते हो या जो इसको देखता है उसको देह कहते हो । दिखने वाला देह है कि देखने वाला देह है ?
पहले प्रश्न समझो ! अरे भाई ! 'दिखना' शब्द है वह देह के लिए आता है या देखने वाले के लिए आता है ? देह अधिष्ठान है या अध्यास ? अध्यास । इण्डा अध्यास है कि अधिष्ठान ! अध्यास । इसी तरह देह अध्यास है कि अधिष्ठान ? अध्यास तो क्या अध्यास दिखता है ? अरे भाई, आभूषण देखते हो कि सोना ? सोना । तो आकार प्रकार देह है कि जो दिख रहा है वह देह है? आकार- प्रकार । यानी अगर यह लकड़ी लम्बी न हो तो डण्डा रहेगा क्या ? लम्बायमान होने से ही तो इसका नाम डण्डा पड़ा। याने आकार- प्रकार से । तो यदि इसमें आकार प्रकार न हो तो देह रहेगा क्या ? तो फिर मगर तारीफ यह है कि लम्बेपन भी लकड़ी है। तो इसी प्रकार 'में' आत्मा आकार-प्रकार में भी तो हूं। तो मैं ही तो हूं। तो 'मैं' दिख रहा हूं कि शरीर दिख रहा है ? यह अध्यात्म है। बुद्धि का विषय थोड़े ही है। बुद्धि तो साहित्य को ग्रहण करती है। यहां तो साक्षात्कार कराया जा रहा है। "सेल्फ रियलाइजेशन" है यह ।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में-
'आश्चर्यवत्पश्यति कश्चेिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः ।
आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् । २९।'
(श्रीमद्भगवतद्गीता अ. २ श्लोक २९)
कोई इसे आश्चर्यदत् देखता है, कोई आश्चर्यवत् सुनता है कोई आश्चर्य के समान कहता है। परन्तु आश्चर्य है उसको जो इसे देखता है और कथन करता है उसको भी आश्चर्य है। क्यों ? इसलिए कि महासागर में गोता (डुबकी) लगाकर उसके अंदर से अनमोल रत्न को निकालकर जो व्यक्त करता है वाणी के द्वारा आश्चर्य है। इसका कथन करना हरएक का काम नहीं है भैय्या । एक श्रुति आती है-
'श्रवणायापि बहुनिर्यो न लम्यः श्रृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः ।
आश्चर्योवक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ।७।'
(कठो. उप.नं. ७)
ब्रम्ह विद्या के सुनने वाले बहुत नहीं है। बाजार नहीं लगा है और सुनने वालों में से जानने वाले भी बहुत नहीं है। एक तो सुनने वाले बहुत कम हैं इसके, दूसरा प्रश्न होता है, कि स्वामीजी ! आपके प्रवचन में तो बहुत भीड़ होती है। भैय्या ! ब्रह्मविद्या की यह महिम्मा है कि पशु-पक्षी स्थावर जंगम सभी समाधिस्थ हो जाते हैं और यह स्वानुभूति है परन्तु श्रुत्ति भगवती का यह कहना बिल्कुल सत्य है। एक तो सुनने वाले कम हैं और सुनने वालों में से जानने वाले बहुत कम हैं। दूसरा प्रश्नः - स्वामी जी आपके ब्रम्ह निरुपण में हजारों बैठे रहते हैं। उस समय तो उन हजारों सुनने वालों में से बहुत कम होंगे जो स्वरूपस्थ न हो जाते हों चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो । यह अध्यात्म विद्या का जो प्रवक्ता है उसकी शक्ति है उसका संकल्प है। सारा विश्व समाधिस्थ हो सकता है कोई आश्चर्य नहीं है। हां जी ? आ जाओ विषय पर जिसका निरूपण हो रहा है जिस ब्रम्ह तत्व का, जिस आत्म तत्व का निरूपण किया जा रहा है। निरूपण कर्त्ता वही है। साहित्य का निरूपण तो जीव देश से होता है। बुद्धि का विलास है, बुद्धिगद है। सुन्दर-सुन्दर शब्दों का विन्यास, शब्दाडंबर, बुद्धि का विषय है और जीव देश से हो सकता है साहित्य का निरूपण । परन्तु जो आत्म तत्व का निरूपण है, अरे प्रेक्टिकल है थ्योरी नहीं है। प्रेक्टिकल अनुभूति वह तो स्वयं से हो सकती है और स्वयं ही इसको करेगा, दूसरा कौन कर सकता है ? अरे ! एक चीज़ और है, जितने यहां बैठे हो पंडाल में दोनों समाज में तुभ सबों को अपने आप से भिन्न मानकर कितना भी मत्या पटकू तुम्हें समझाने के लिए तो कभी समझ में न आएगा। हर हालत से हम स्वरूपपस्थ होकर कहते हैं तब तुम्हारे समझ में आता है। यह तो मानव जगत है, पशु जगत में ले चलो हमें, उन्हें भी ऐसा ही बोध होगा आकार-प्रकार भले पशु का है मगर में ही तो हूं। तो फिर देर ही नहीं समझाने में। तो भैय्या ! लम्बायमान को डण्डा कहोगे न । तो यह जो आकार-प्रकार है तो फिर उसमे देह की कल्पना की गई है। यह देह है हां फिर दूसरी कोटि- अरे देह-देह-है, कि है-देह है ? आभूषण-आभूषण है कि सोना आभूषण है ? सोना आभूषण । तो फिर 'देह-'देह है' कि 'हैं'-देह है ? 'है' देह 'है' इस इस प्रकार के बोध में देहाभिमान का नाश हो जाता है और पहली बात यह है कि कोई चीज पैदा ही नहीं होती । वाह! हां, जी ।
"न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते ।
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्त्र किंचिन्न जायते ।'७१।
(गौ. पा. कारि. अलातशांति प्र. मंत्र सं. ॥७१॥)
यही उत्तम सत्य है कि कोई चीज पैदा ही नहीं होती। वाह ! हां जी ! फिर - तो जो दिख रहा है 'दिखने' को 'दिखना' देखते हो कि दिखने को देखना देखते हो ! जो दिख रहा है तो दिखने वाला देखने को देखता है जो दिखता है तो दिखने को देखना देखते हो कि दिखता क्या है ? देह तो हुआ दिखना । तो फिर देह को देह देखता है कि देह को मैं देखता हूं । देह को मैं देखता हूं । 'देह' को देह तो नहीं देखता है देह' को 'में' देखता हूं। ठीक है देह से भिन्न होकर देह को देखता हूं या दह ही होकर दह को देखता हूं। देह से भिन्न हो जाऊं तो देह नहीं । डण्ड से लकड़ी अलग कर लो डण्डा नहीं, लकड़ी अगर डण्डे से भिन्न हो तो डण्डा नहीं । भिन्नाभिन्न हो तो डण्डा नहीं इसलिए लकड़ी ही डण्डा है। तो यदि देह से में भिन्न हूं तो देह नहीं क्योंकि अधिष्ठान से भिन्न होकर रहेगा कहां जबकि लकड़ी ही दिख रही है। तो मैं इसमें (शरीर) अलग हो जाऊं तो यह रहेगा कहां । भिन्न हूं तो देह नहीं, अभिन्न हूं तो देह नहीं। भिन्नाभिन्न हूं तो देह नहीं। तो देह देखते हो तो देह होकर ही देह को देखता हूं जिसको भी मैं देखता हूं वही होकर में उसको देखता हूँ और यह तारीफ है कि मुझ भगवान 'आत्मा' को कोई नहीं देख पाता । जब वही होकर उसको मैं जानता हूं तो मुझे कौन देख सकता है। इसलिए मुझ भगवान आत्मा की ओर किसो की दृष्टि नहीं जाती। इसलिए में देह नहीं। 'मैं' भगवान आत्मा की ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती । इसलिए में देह नहीं। मैं भगवान है । 'मे इतना ठोस हूं. इतना घन हूं कि किसी का दृष्टिपात नहीं होता। सबकी दृष्टि विशेष की ओर जाती है सामान्य की ओर नहीं जाती। विशेष की तरफ जाती है, सामान्य की तरफ नहीं जाती है क्योंकि विशेष परिच्छिन्न होता है और सामान्य सर्व होता है। विशेष किसी के अनुकूल होता है तो किसी के प्रतिकूल । परन्तु सामान्य सर्वे में सर्व है।
"यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यत्सर्वं सर्वतश्चयत् ।
यच्च सर्व मयं नित्यं तस्मैसर्वात्मने नमः ॥"
मैं सर्व हूँ । आँख में आँख रूप से हूँ, कान में कान रूप से हैं। जिव्हा में जिव्हा रूप में हूँ। अरे ! जिसमें हूँ उसमें वही रूप हूँ। लकड़ी डण्डा रूप से है, यह थोडे है कि लकड़ी अलग होय और डण्डा अलग होय । तो फिर जिसमें हूँ, उसी रूप से जब उसमें हूँ . तो फिर एक और दो का सवाल ही पैदा नहीं होता ।
'देह' को यदि विकल्प कहो तब देह नहीं और वस्तु कहो तब देह नहीं । डण्डे को अगर विकल कहो तो डण्डा नहीं और लकड़ी कहो तो डण्डा नहीं इसी तरह देह को विकल्प कहो तो देह नहीं वस्तु कहो तो देह नहीं। इसी तरह सारे प्रपंच को विकल्प कहो तो प्रपंच नहीं और वस्तु कहो तो प्रपंच नहीं। तो अगर देहादिक प्रपंच का अस्तित्व यदि है तब तो एक और नाना की कल्पना हो सकती है और जब है ही नहीं तो नानात्व भाव और एकत्व भाव रहेंगे कहाँ ? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था जिज्ञासुओं से कि 'है' देह है कि 'देह' देह है। वह हल नहीं किया गया है। "है" देह है या 'देह' देह है ? एक । 'है' देह है कि 'देह' 'है' है। शिव। 'हैं' देह है। 'देह' देह नहीं है क्योंकि बिना 'हैं' के 'देह' नहीं है इसलिए 'है' देह है, देह यह नहीं है। अस्तिव ही तो है। 'है' देह है कि 'वह' देह है। 'लकड़ी' डण्डा है कि 'डण्डा' लकड़ी है ? 'लकड़ी' डण्डा है क्योंकि बिना लकड़ी के डण्डा 'नहीं' है। अच्छा । ठीक उसी तरह 'है' देह है कि 'देह' 'है' है ? 'है' देह है। 'है' का नाम देह है कि 'है' का रूप देह है। न है का 'नाम' देह है न है का 'रूप' देह है जब कि 'है' ही देह है। देह देश से देह है कि 'है' देश से देह है। 'स्वर्ण' देश से आभूषण है कि 'आभूषण' देश से आभूषण है। 'मैं' भगवान आत्मा अधिष्ठान आत्मा जब देखता हूँ तो मैं जिस समय जिस चीज को देखता हूँ उसको वही हो कर देखता हूँ या उससे भिन्न होकर देखता हूँ। उससे भिन्न होने पर तो वह चीज़ ही नहीं रहती । देखने-सुनने का प्रश्न ही कहाँ ? अब अनुभव करो । 'शिव' जिस समय किसी भी विषय का 'मैं' आत्मा अनुभव करता हूँ उस समय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हूँ यदि विषयों में जिस विषय का भी अनुभव करता हूँ। इसका क्या प्रमाण है कि उसका मैं वही होकर अनुभव करता हूँ। इसका प्रमाण यह है कि- विषय के अनुभव काल में मुझ 'आत्मा' को यह अनुभव नहीं होता कि मैं अनुभव कर रहा हूँ। जब क्रिया का अनुभव नहीं होता तो अनुभव जो कर्म है, वह कहाँ जब क्रिया और कर्म नहीं तो कर्ता कहाँ ? क्या प्रमाण है कि में जिसका अनुभव करता हूँ वही होकर अनुभव करता हूँ। यह मोर्चा है अच्छा ! तो इसका यही प्रमाण है कि किसी विषय के अनुभव काल में मुझ आत्मा की अमुक विषय का अनुभव कर रहा हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता । न तो विषय का अनुभव होता और न 'मैं' अनुभव कर रहा हूँ इस क्रिया का अनुभव होता है तो क्रिया कर्म के अभाव में कत्र्ता का भी अभाव होता है। यदि जिस विषय का अनुभव करता हूँ वह विषय मुझे आत्मा से भिन्न है सर्वथा, तो उसके अनुभव काल में विषय का अनुभव हो । इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिसको में अनुभव करता हूँ वही होकर करता हूँ वही होकर अनुभव करता हूँ। इसी तरह जब 'में' देह को देखता हूँ तो देह होकर ही देह को देखता हूँ। मगर देह के दर्शन काल में मुझे देह रूप दृश्य की अनुभूति नहीं होती। इसलिए देह ही नहीं है। प्रपच ही नहीं हैं। शब्दादिक विषय ही नहीं है। न आत्मभाव से नाना है न स्वयं करके नाना है। न पृथक न अपूपृथक है और हम थोड़े ही कहते हैं श्रुति कहती है- बड़े-बड़े तत्त्व वेत्ताओं ने कहा है ऐसा । कैसे तत्त्ववेत्ता ? बड़े-बड़े बीतराग महापुरुष । आत्म नैष्ठिक पुरुषों ने इस आत्मा को देखा है उनका ऐसा कहना है। दूसरे, क्या जान सकते हैं ? हाँ जी, अनुभव करो। इस डण्डे से, डण्डे को डण्डा मानकर इससे अपने आप को अलग करके 'मैं' इसका द्रष्टा हूँ और यह मेरा दृश्य है, इस भेद बुद्धि को लेकर डण्डा देखता हूँ तब तो डण्डा है नहीं तो मैं हूँ। इसी तरह सब विषयों को समझ लो यानी किसी विषय के अनुभव काल में विषयानुभूति मुझ आत्मा को नहीं होती तो विषयानुभूति का अभाव ही तो आत्मानुभूति है शब्द, रूप, रस गंध और स्पर्श यानी किमी विषय के अनुभव काल में अनुभव करने वाले को मुझ आत्मा को उस समय विषय का अनुभव नहीं होता तो विषय का अनुभव नहीं होता तो विषयानु- भूति के अभाव में क्या अनुभव होता है ? यही आत्मानुभूति है। आगे पीछे तो विषय का विकल्प होगा मगर ऐन वक्त में अनुभव काल में उस विषय की अनुभूति नहीं होती। जब कि नहीं होती तो क्या अनुभव होता है उस समय ? अरे ! वही तो स्वानुभूति है जो वाणो गम्य नहीं है। विजयानुभूति का अभाव ही स्वरूपानुभूति है।
अब १२ बज रहे हैं मध्यावकाश के बाद २ बजे से प्रवचन पुनः प्रारम्भ होगा ।
समय २ से ४ बजे तक
तृण से आदि ब्रम्हा पर्यन्त सारा जगत प्रपंच 'मैं' आत्मा हूं। मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है इसके ऊपर एक कारिका कही जाती है-
'नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन ।
न पृथङ् नापृथक्किंचिदिति तत्वविदो विदुः ।'
(गौ. पा. कारि. वैतथ्य प्रकरण म स. ।३४।)
यह जो अनेकत्व प्रपंच है, न आत्मभाव करके अनेकता है और न स्वयं करके अनेकता है यानी न एक करके अनेक है न अनेक करके अनेक है। प्रपंच में ही अनेकता का विकल्प होता है। न प्रपंच करके नानात्व भाव है न मुझ आत्मा करके नानात्व भाव है । न यह भिन्न है न अभिन्न है ।
'जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः एकोर्नावश
तिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ।' (३)
(गौ. पा. कारि. आगम प्र. मंत्र सं. ।।३।।)
स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति
मुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः ।४।
(गो. पा. कारि. आग. प्र.)
यत्र सुप्तों न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति तत्सुषुप्तम् ।
सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ।५।
(गौ. पा. कारि. आगम प्रकरण मं. सं. ।५।)
'नान्तः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् ।
अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षण मंचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं
प्रपंचोपशम शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ।७।'
(गो. पा. का. आग. प्र. म. सं ।७।)
ऐसा जो स्वस्वरूप आत्मा है वह जानने योग्य है। न में भीतर को जानता हूं न मैं बाहर को जानता हूं और न भीतर बाहर को जानता हूं गरज यह है कि बाहर-भीतर हो तब तो में जानू । न में भीतर को जानता हूं न मैं बाहर को जानता हूं। देखो आत्मा का विशेषण प्रज्ञानम् ब्रम्ह दिया है- प्रज्ञानम् का अर्थ होता है तत्काल ही जो जाने । गरज यह है कि जिसको जानने के लिए काल की सीमा न हो। जिसको जानने के लिए समय की पाबंदी न हो कि 'में' आत्मा कितनी जल्दी जानता हूं । (फूल की माला दिखा- कर) कितनी जल्दी जानता हूं। एक सेकेंड या पाव सेकेंड । किसी भी दोज को जानने के लिए मुझ आत्मा को काल की सीमा नहीं है। यह प्रज्ञानम् का अर्थ है। तत्काल ही जाने और दूसरी चीज यह है कि जानने के लिए काल की सीमा नहीं है और किसी चीज को जानने के लिए कोई जरिया नहीं, यानी कोई उपकरण नहीं । किसी के जरिये 'मैं' आत्मा नहीं जानता। हां जो मैं जानता हूँ उसे प्रकट करने के लिए भले ही उपकरण की जरूरत पड़ती है। मगर जानने के लिए किसी उपकरण की मुझ आत्मा को जरूरत नहीं होती । तो गरज यह है कि मुझ आत्मा को किसी चीज को जानने के लिए न कोई काल की सीमा है न उपकरण की जरूरत है कोई चीज हो तब में जानू । जैसे सो जाने पर सुषुप्ति-गाढ़ी निद्रा में मैं आनन्द का अनुभव करता हूं। तो आनन्द का अनुभव तो में करता हूं परन्तु बड़ा आनन्द आ रहा है इसे जाहिर करने के लिए मुझ आत्मा के पास कोई जरिया नहीं होता। जागृत अवस्था में मन जब आता है, तब इन्द्रियां भी आ जाती हैं तब में बताता हू कि बड़ा आनन्द आया । मगर जिस वक्त में आनन्द का अनुभव करता हूं उस वक्त किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती । में किसी भी विषय का अनुभव कितनी जल्दी करता हूं। किसी उप- करण की जरूरत नहीं है काल की सीमा नहीं ।
न में भीतर को जानता हूं न बाहर को जानता हूं । बाहर- भीतर का विकल्प तब हो, जब मुझ आत्मा के सामने कोई और हो कोई घेरा हो, कोई कम्पाउन्ड हो या चारों तरफ दीवाल खीची हुई हो तब तो कहीं मैं बाहर भीतर को जानता । मुझ आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं तो मैं बाहर को जानता हूं न भीतर को जानता हूं । न भीतर बाहर दोनों को जानता हूं । उस वक्त देह का अभाव हो चुका है। यानी देह का जब विकल्प करोगे कि देह है तब बाहर भीतर का विकल्प होगा । जब देह का विकल्पाभाव हो गया तो बाहर भीतर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और न में प्रज्ञान घन है क्योंकि जब जानने की कोई चीज हो मुझ आत्मा के सिवाय तब न में जानू ? इसलिए मैं प्रज्ञानघन भी नहीं । जब ज्ञेय नहीं तो ज्ञाता कौन होगा ।
"नान्तः प्रज्ञं ।
'मैं' आत्मा अदृष्ट हूं । अदृष्ट कहते हैं जो देखा न जाय और जिसको कोई न देख सके । न में किसी करके द्रष्टा हूं न स्वयं करके दृष्ट हूं । न तो 'मैं' इन्द्रियों करके दृष्ट हूं और न स्वयं करके देखा जाता हूं । इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ।
'न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदें वैस्तपसा कर्मणा वा ।
ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ।८।'
(मुण्डक उप. मं. (८))
इन्द्रियों के द्वारा में ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं अदृष्ट हूं । यह भाव तो ठीक समझ में आ जाता है कि 'मुझ' आत्मा को कोई इन्द्रिय स्पर्श नहीं कर सकती, परन्तु क्या मैं भी अपने आपको नहीं देखता । और कोई बतादे कि अपने आपको क्या देखता है कि में क्या देखता हूं और जो देखते हो वह में हूं नहीं। यह जो देखते हो क्योंकि ऐसा 'देखा जाता है' जैसा नहीं देखा जाता अगर में ऐसा हूं तो अदृष्ट नहीं । 'मैं' ऐसा हूं तो दृष्ट हू और 'मैं' जैसा हू तो दृष्ट नहीं। मैं ऐसा हूं तो मुझ आत्मा का विशषण अदृष्ट न होगा। अगर मैं कहूं कि 'जैसा' हूं तो दृष्ट न होगा। क्योंकि 'जैसा' दृष्ट नहीं होता दृष्ट तो 'ऐसा' ही होता है। इसलिए भय्या! 'में' न किसों और करके दृष्ट हूं और न स्वयं करके दृष्ट हूं इसलिए कि में 'अदृष्ट' हूं। जी हाँ- जिस वक्त में अपने आप को देखने चलता हूँ तो में खुद ही खो जाता हूँ। जिस वक्त में अपने आपको देखने चलता हूं तो देखने का विकल्प ही शान्त हो जाता है तो देखे किसको और कौन देखे । कहते हैं भाई, आत्म दर्शन करो । अपने आपको देखो, अपने आपको पहिचानो तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है जब में अपने देखने की चीज ही नहीं हूं न किसी और के द्वारा देखा जाता हूं तो सन्त महात्मा जन क्यों ऐसा कहते हैं कि अपने आपको देखो, अपने आपको पहिचानो। तो फिर आत्म दर्शन का क्या मतलब तो आत्म दर्शन का यही मतलब है कि कुछ भी न देखना यही आत्मदर्शन है, कुछ भी न जानना यही आत्म ज्ञान है। किसी किस्म का अनुभव न होना यही आत्मानुभूति है। क्योकि में अदृष्ट हूँ। यानी कुछ भी न देखना, तो कुछ के न देखने पर रहता कौन है ? कुछ भी न देखना । देखो देखने-दिखाने का जानने-जनाने का सुनने-सुनाने का जो विकल्प है। यह कल्पना स्वदेश की है कि परदेश की ? 'स्व' माने स्वरूप आत्मा में न जानना है, न देखना है न दिखाना है, न सुनना है न सुनाना है क्योंकि में अदृष्ट हूँ । अनुभव करो - यह तो नकद धर्म है रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का चैक है। में हूँ यह 'भाव' 'वाचक' शब्द है कि 'संज्ञा' वाचक शब्द है ? "में हूँ" अब 'मे' को देखने चलो। किसी के दिखने पर 'मैं' दिखता हूँ कि किसी के न दिखने पर 'में' दिखता हूँ। कोई चीज़ दिखती है उसकी अपेक्षा से दिखता हूँ या नहीं दिखती उसकी अपेक्षा से दिखता हैं? भाई देखो न- 'में' आत्मा से भिन्न को दिखना कहते हो तो, ऐसा कहना तो इन्द्रियों का विषय है। इन्द्रियाँ जिन-जिन विषयों को ग्रहण करती हैं उन-उन विषयों के लिए तो दिखना आता है तो किसी के दिखने से में दिखता हूं कि किसी के न दिखने से 'मैं' दिखता हूं । किसी चोज़ को 'मैं' देखता हूं तो 'मैं' नहीं दिखता और 'में' को देखता हूं तो दिखने वाला नहीं दिखता । 'देह' को देखता हूं तो 'मैं' नहीं दिखता, और 'मैं' को देखता हूं तो देह नहीं दिखता । अनुभव करने चलो। देह को देखता हूं तो 'मैं' नहीं दिखता 'मैं' को देखता हूं तो देह नहीं दिखता। जिस वक्त अपने देह को देखते हो तो क्या यह भान होता है कि यह देह है और यह 'मैं' हूं। 'नहीं' में को देखता हूं तो देह नहीं दिखता । इससे सिद्ध होता है कि 'मैं' और 'देह' दो चीज नहीं है। अनुभव करो । मेरा मन गया, मेरा मन आया, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन चचल है। तो 'मन' को जब देखता हूं तो यह भान होता हैकि यह मन है और यह मैं हूं। तो फिर किस करके में दृष्ट हूं ? जब मुझ आत्मा से कोई भिन्न हो तब तो वह मुझ आत्मा को देखे तो जिस चीज को में देखता हूं, उस चीज के दर्शनकाल में मुझ आत्मा अपने आप को यह अनुभव नहीं होता कि यह अमुक हैं और 'मैं' उसका द्रष्टा हूँ । तो देह को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता । क्योकि दिखें कैसे, जबकि में देह में देह रूप से हूं, सर्व में सर्वं रूप से हूं तो सर्वं का अनुभव काल में सर्व का मुझ से भिन्न अनुभव नहीं हो सकता इसलिए में आत्मा अदृष्ट हूं। अपने आपको देखने चलो, पता लगाओ तो किसी प्राच को अनुभूति नहीं होती । अपने आप ही रह जाता हूं और प्रपंच का अनुभव करने चलो, देखने चलो तो फिर 'मैं' आत्मा का अनुभव नहीं होता क्योंकि एक ही रहेगा। चाहे अपने आपको देह कहाँ पाहे अपने आप को प्रपंच कहो । सीधी बात है मेला को देखते दो तो में नहीं दिखला 'मैं' को देखता हूं तो मेला नहीं दिखता । जगत प्रपंच की सृष्टि होती है यह तो अभाव में अभिनिवेश है यानी है नहीं बाहमख्वाह उसे मान लेता है कि यह चीज है क्योंकि में आत्मा अदृष्ट हूं। अरे ! यही तो आत्मदर्शन है यार । न अपने से भिन्न की प्रतीति हो न अपने से अभिन्न की प्रतीति हो न अपने आप से भिन्नाभिन्न की प्रतीति हो ।
"प्रतीति का अभाव ही आत्म दर्शन है।"
यानी देह की प्रतीति का अभाव हो गया न । ऐसो बात त नहीं है कि वर्तमान हाथ पैर वाला आत्मा आ करके खड़ा हो जाब और मै देखूं तब समझू कि मुझे आत्म दर्शन हुआ है। फर्ज कर कोई आ भी जाय सामने तो उसको देखता हूं तो में नहीं दिखता 'में' को देखता हूं तो वह नहीं दिखता और अगर दिखता तो फिर बतावें हम । अपने में की यादगारी रख कर-डण्डा देखो 'मैं' हूं इसकी यादगारी में यानी इसके स्मरण में डण्डा देव दिखता है ? और 'डण्डे' की यादगारी में अपने आपको देखो । वह विकट मामला है। हां, ये बात । अध्यात्म तत्व है यह। मेंहू इसक यादगारी में डण्डा नहीं दिखता । 'मैं' हू इस गुक्ति से अगर ह देखते हो तो डण्डा नहीं दिखता तो यह प्रतीति क्या है? मैं हू इसक यादगारी में डण्डे की प्रतीति नहीं होती । अब जो प्रतीति होतो वह तो 'मे' हूं। यानी 'देह' को देखता हूं तो 'में' नहीं दिखत और 'मैं' को देखता हूं तो देह नही दिखता । अरे हो तब तो दि अरे ! देह तो विकल्प है।
अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते ।
द्वयाभावं स बुद्ध्वैव निर्नानिमित्तो न जायते । ७५।
(गौ. पा. कारि. अलात शा. प्र. मंत्र सं. ।।७५।।)
अभाव में जो होने का अभिनिवेश है तो जानने पर द्वैत का अभाव है इसलिए कोई चीज़ पैदा होती ही नहीं क्योंकि में अदृष्ट हूं हां जी ।
नान्तः प्रज्ञं …………………….. स विज्ञेयः
अब यहां जरा ठिठक जाओ और में हूं इसका पता लगाओ । में क्या हूं ? इसका पता नहीं लगता में कहां हूं इसका पता नहीं लगता । यहां पर केवल सत्ता मात्र है, सिर्फ सत्ता की ही अनुभूति होती है। इस पद में, अस्तित्व पद में देखो - जो अपने आपको साढ़े तीन हाथ का मानता है यही मैं हूं, तब उसको साढ़े तीन हाथ के देह से उसको अपने 'मैं' का भान नहीं होता और कहते हैं- कि 'में' आत्मा नित्य हूं या अनित्य हूं, सत् हूं या असत् हूं। जड़ हूं या चेतन हूं, व्यापक हूं या सीमित हूं ।
"नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताशाश्वताभिधा ।
यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्त्र नोच्यते ॥६०॥
(गौ. पा. कारि. अला. शा. प्र. मं सं. । ६०।)
जहाँ वाणी जाही नहीं सकती तो सत्य और असत्य का विकल्प कहाँ कि में ऐसा हूं और ऐसा नहीं हूं। जो वाणी का विषय है नहीं, उस ब्रम्ह सनातन तत्व के लिए किसी किस्म का विकल्प है ही नहीं कि वह ऐसा है और ऐसा नहीं है। इसीलिए कि मैं आत्मा अदृष्ट हूं। मैं शाश्वत हूं कि अशाश्वत हूं कोई विकल्प नहीं है। तब फिर क्या कहा जा सकता है कि मैं आत्मा इस प्रकार का हूं। तो फिर बया का विकल्प ही नहीं है। मन को देखता हूँ तो में नहीं दिखता और 'मैं' को देखता हूं तो मन नहीं दिखता । जिस वक्त तुम अपने मन का अनुभव करते हो, मन के आने का जाने का मन की स्थिरता का मन की चंचलता का, तो क्या अपने मैं का अनुभव करते हो। मन के दर्शन काल में? नहीं होता। तो फिर इसका हल क्या है अरे ! मन नहीं है भाई, देह नहीं है, प्रपंच नहीं, जगत नहीं, माया नहीं । अरे ! 'मैं' आत्मा ही तो हूं। पहले तो मुझ आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं और यदि कुछ है भी तो फिर मैं ही हूं जो नाना नाम रूपों में अभिव्यक्त हो रहा हूं । परन्तु नाना नाम रूपों में अभिव्यक्त होने के बावजूद भी में अदृष्ट हूं। अब इसे समझना है?
'मैं' आत्मा नाना नाम रूपों में दिखने के बावजूद तब भी अदृष्ट हूं । कैसे ? जब नाना नाम रूपों को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता । क्योंकि नाना नाम रूपों से में अलग जैसा होऊं तब न दिखूं । नाना नाम रूपों को देखूं तो 'मै' नहीं दिखता और मैं को देखूँ तो नाना नाम रूप नहीं दिखते । इसीलिए तो मैं अदृष्ट हूँ तो मेरे ख्याल से अब तो मन से किसी किस्म का डर नहीं रहा । नहीं रहा तो अपने घर में बैठो । हो जाओ स्वरूपस्थ लेलो इनका आनंद फिर आगे की बात बतावें । अनभ्यास में बैठ जाओ अभी जिस अनुभूति पद में बैठाए गए हो वह स्वस्थ पद है। क्योंकि प्रपंच का तो सर्वथा अभाव है । अब यहां एक प्रश्न होता है कि जब मैं प्रंपच को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता और मैं को देखता हू तो प्रपंच नहीं दिखता । तो प्रपंच किसको कहते हैं? यह प्रश्न है जिसका पता लगाने पर पता न लगे। जिसका अनुभव करने पर अनुभव न होय उसका नाम प्रपंच है। अरे ! भाई डण्डा उसको कहते हैं कि पता लगाने पर डण्डा न मिले संसार इसी को कहते हैं ।
"मैं तोहि अब जान्यों संसार ......।"
इसका मतलब यह है कि अरे यह 'में' हूँ यह 'तू' है। ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, कछु न निकसत सार। कदली कहते हैं केलेको। केलेका जो खंभा होता है उसे देखो- तो बड़ा सुन्दर मालूम पड़ता हैं। मगर एक-एक छिलका निकालते जाओ। जो असार है, उसका नाम संसार है ।
"ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, कछु न निकसत सार "
"मैं तोहि अब जान्यों संसार …………………….''
अब प्रश्न होता है कि प्रपंच को देखता हूँ तो मैं नहीं दिखता। मैं को देखता हूँ तो प्रपंच नहीं दिखता । तो प्रपंच का क्या स्वरूप है? देखने चलो तो जो नहीं मिलता उसका नाम प्रपंच है। तो फिर बाद में जो प्रतीति होती है यह क्या है ? यह दूसरा प्रश्न है। बाद में प्रतीति होती है वह क्या है ? तो प्रतीति प्रपंच की नहीं होती । संसार तो विकल्प था वह देखने पर नहीं मिला तो बाद में जो रह गया वह क्या है ? तो वही तो सत्ता है, वही तो अस्तित्व है। जी हाँ, संसार तो वाणी से कहा जाता है कि ऐसा नाम है, ऐसा रूप है। मगर जब देखने चलते हो तो न नाम का पता चले न रूप का पता चले । प्रतीय मान रह जाता है, भास ही भास रह जाता है, दूसरे शब्दों में ऐसा कहो- जिसको इन्द्रियाँ विषय करें उसका नाम ससार है और जिसका विषय में करता हूँ, जिसका अनुभव में करता हैं तो वह तो में ही हूँ। परन्तु हाँ यह बात जरूर है कि जो 'मैं' आत्मा हूँ तो न में किसी और करके देखा जाता हूँ न में अपने आप बारके देखा जाता हूँ क्योंकि मैं अदृष्ट हूँ। लकड़ी है यह ओस्तत्व । छकड़ी', डण्डा नहीं है, इसी प्रकार देह 'है' यह जो "है" अस्तित्व, हस्ती वजूद तो यह अस्तित्व है भास रहा है। यह 'है' है जो भास रहा है। अब इस भास का ही नाम रख दिया गया संसार। अस्तित्व पर ही संसार की कल्पना की गई ? फर्जी ! क्योंकि मैं आत्मा अदृष्ट हूँ। अब मेरी समझ में अनभ्यास के अभ्यास में बैठने से जो आवाज आती है उस आवाज से हृदय को ग्लानि होती थी। नहीं होनी चाहिए । अगर यह जम गया, इसकी अनुभूति हो चुकी है तो नहीं होगी। जिसकी अनुभूति कच्ची होगी तो नहीं होनी चाहिए आजकल, रेडियो में चाहिए का भरमार है। संसद में चारों तरफ चाहिए-चाहिए । ऐसा होगा कहने की हिम्मत नहीं होती । ऐसा होना चाहिए । तो गरज यह है कि अनभ्यास के अभ्यास में बैठन पर जो शब्दादिक विषयों से जो भय लगता था अब नहीं होन चाहिए । जब कल दस बजे से सूपा पीटा जा रहा है। यह है आत्म चितन है यही ब्रह्म चितन है और यही भगवान ध्यान है। बस ! क्योंकि- अदृष्टम् । तो
नान्तःप्रज्ञं सः …………………………. विज्ञेय ।
दूसरा विशेषण आता है, भगवान आत्मा का अग्राह्यम यान जिसका ग्रहण न होय । यह सब भगवान आत्मा का विशेषण दिय गया है न तो इन्द्रियों करके जो ग्राह्य न हो और स्वयं अपने आप करके भी जो ग्राह्य न हो। यह भी बात है। इन्द्रियों करके ज ग्रहण न किया जाय । वाणी जहाँ से वापस आ जाती है। वाप अभिव्यक्त नहीं कर सकती कि 'मैं' ऐसा हूँ । जो वाणी द्वारा ग्रह न किया जा सके मन की वहाँ पहुँच ही नही है।
"दृष्टेः द्रष्टारम् न पश्येत् ।"
('वृहदारण्यश्रुति')
दृष्टि के द्रष्टा को दृष्टि क्या देख सकती है। बयान नह किया जा सकता जिसका लॉ बयाँ । मगर क्यों लॉ बयाँ ? लॉ बयाँ- देखो कहते तो सभी हैं, भगवान आत्मा मन वाणी का विषय नहीं * मगर इसका प्रत्यक्षीकरण (स्पष्टी करण) कोई नहीं करता। दृद्धि क्यों निश्चय नहीं कर सकती, चित्त क्यों चितन नहीं कर सकता, इसका स्पष्टीकरण नहीं है।
दृष्टि उसको देखती है जो दृष्टि से दूर होता है। बड़े-बड़े "आईज स्पेशलिस्ट" हैं आंख के डाक्टर। उसकी आंखे ठीक है और बाकी में दोष है। मगर यहाँ तक (स्वामी जी हाथ क्रमशः आंख के नजदीक ले जा रहे है) आँख किताब देख सकती है, मगर अब आंख क्या देखेगी ? मैं आत्मा आँख से इतना नजदीक हूँ कि में आँख की आँख हूँ। जब में आँख की आँख हूँ तो मुझको आज क्या देख सकती है यह स्पष्टीकरण है। जब मैं वाणी की वाणी हूँ, घ्राण का घ्राण हूँ ।
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य ।
याण. चक्षुषश्चक्षुरति मुच्य धोराः प्रत्यास्मा ल्लोकादमृताभवन्ति ।
(केनोपनिषद् खंड १ मं० सं० ॥२॥)
जो दृष्टि की दृष्टि है जो मन का मन है, जो वाणी की वाणी है जो आँख की आँख है, जो प्राणों के प्राण हैं।
"प्राण, प्राण के जीव के जिय सुख के मुखराम" सर्व में सर्व होने के कारण, सर्व करके मैं आत्मा 'अग्राह्य' हूँ । कोई ग्रहण नहीं कर सकता मुझ भगवान आत्मा को । यदि सर्व से मैं आत्मा दूर होऊँ और सर्व से मैं आत्मा विलक्षण होऊँ अरे ! में इतना घुला-मिला हे सर्व से कि मुझ आत्मा में कोई विशेषता नहीं यही मुझ आत्मा को विशेषता हैं कि में किसी से विशेष नहीं हूँ इसलिए मैं 'आत्मा' अग्राह्य हूँ। जी हाँ ! कोई भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं । यही मुझ भगवान आत्मा की विशेषता है। तो फिर यह करके सर्व का सर्व ही हूँ। सर्व में सर्व हूँ और सर्व करके सर्व है इसलिए में अग्राह्य हूं। तो ग्राह्य और अग्राह्य दोनों ही विकल्प और मुझ आत्म देश में न ग्राह्य है और न अग्राह्य है। न ग्राह करके ग्राह्य हूँ न अग्राह्य करके ग्राह्य हूँ। ग्राह्य और अग्रा करके ग्राह्य न होने के कारण में आत्मा अग्राह्य हूँ। जब आत्मा किसी से विलक्षण होऊँ तब में विशेष होऊँ जब मैं विशेष होऊँ तो किसी का ग्राह्य हौऊँ । फिर समझो । जब में आत्म किसी से विलक्षण होऊँ और किसी से विशेष होऊँ क्योंकि विलक्षण और विशेष के ही लिए ग्रहण करने का विकल्प होता है। साधन किया जाता है। जब मैं किसी से विलक्षण नहीं और किसी के विशेष नहीं । तो फिर ग्रहण कौन करे मुझको । 'मैं' आत्मा ग्राह किसका ? और मैं स्वयं आत्मा अपने आप करके अग्राह्य क्यों हूँ क्योंकि मुझे जरूरत क्या है ? कि मैं अपने आपको ग्रहण कर और ग्रहण की अपेक्षा त्याग होता है। यदि आज मैं ग्राह्य हो जाऊँ तो एक दिन त्याज्य हो जाऊँगा । इसीलिए अग्राह्य हूँ। अरे ! जिन्दगी कश्ती ये दरिया पार हो हरगिज न हो।" होके बे परवाह फिर परवाह करना जुर्म है। और लगेगी किनारे कभी कभी । मुबारक हो यह मस्ती खुदा जिसको बख्शे ।
और जो मुझ भगवान आत्मा को ग्रहण करने चलता है मैं ही हो जाता हूँ तो ग्रहण कौन करे । / छुआ-छुई के खेल में बालक चोर बनता है उसको जो छू लेता है। छूत ही बीमारी तो। छुआ-छुई खेल में ऐसा चांस आता है कि एक लड़का चोर बन जाता है और वह चोर लड़का सब लड़कों को छूने के लिए दौड़ता है और चोर से जो छुआ जाता है वह भी जोर हो जाता है इसी तरह भगवान को छूने के लिए जो चला वह भग- बान हो जाता है- “सो जाने जेहि देहु जताई, जानत तुमहि-तुमहि होइ जाई। जो आज दिन तक पढ़ने में नहीं आया कि जो छूने गथा और लौट के बताने के लिए कोई नहीं आया वही हो गया, खतम। वजूद खतम हो गया । जो नदी समुद्र को छूने के लिए चली, समुद्र से मिलने के लिए चली, वह आज तक नहीं बताई कि मैने समुद्र को जाना है। इसी किस्म से जिसने भगवान को पाया, जिसने भगवान आत्मा का दर्शन किया और जो छू लिया वह भगवान हो गया, वह क्या बता सकता है कि भगवान ऐसा है और अगर बताता है तो छुआ नहीं है। अफसाना है। क्योकि अग्राह्यम् ।
अब चार बज रहे हैं, आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है।
ॐ पूर्ण मदः पूर्ण मिदं, पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवाव शिष्यते ।।
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!
तृतीय दिवस का प्रवचन
(बुधवार, दिनांक १४ नवम्बर सन् १९७३समय- १० बजे से १२ बजे ।)
"ओमित्येतदक्षरमिदꣲ᳭ ..... ... ... …… तदप्योंकारएव"
कल के प्रसंग में स्वस्वरूप भगवान आत्मा के जो विशेषण दिये गये हैं- नान्तः प्रज्ञं……
कल इसका विवेचन हुआ था और आज भी है। न में आत्मा बाहर को जानता हूं न में 'आत्मा' भीतर को जानता हूं क्योंकि मुझ आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं तो बाहर भीतर का प्रश्न ही नहीं रहता । अदृष्टम् में अदृष्ट हूं । अदृष्ट का विवेचन कल हो चुका है। 'असाह्यम्' 'में' अग्राह्य हूं। अग्राह्यम् का मतलब यह है कि मुझ भगवान आत्मा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता । मैं अग्राह्य हूं। इन्द्रियों करके ग्राह्य तो में हूं नहीं और स्वयं करके भी अग्राह्य हूं। चोज यह है कि ग्राह्य और अग्राह्य का जो विकल्प है। यह विकल्प प्रपच देश में ही होता है। क्योंकि स्वरूप देश में तो विकल्प है ही नहीं । ग्रहण करने में कोई भी समर्थ नहीं है ।
'यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।'
केनोपनिषद् प्र. खण्ड मंत्र ।।४।।
'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् ।
तदेव ब्रम्ह त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते' ।५।
(केनोपनिषद प्र. खं मंत्र ।५।)
वाणी जिमको व्यक्त करने में समर्थ नहीं है और वाणी को जो प्रकट करता है उसको ही तू सनातन ब्रम्ह जान । इदम रूपा हो। जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रम्ह नहीं है।
मन जिसको ग्रहण नहीं कर सकता, मन जहाँ पर नहीं जा सकता और 'मन' जिसको नहीं जान सकता, मन को जो जानता है मन का जो ज्ञाता है, साक्षी है, उसको ही तू परमात्मा जान । इदं रूप से जिसकी उपासना होती है वह आत्मा नहीं है। इदं कहते हैं यह को। जिस पदार्थ को जानने के लिए यह शब्द लगाया जाय उसको इदम् कहते हैं। वह इदम्गम्य होता है। 'अह' याने 'मैं' होता है वह स्वस्वरूप आत्मा है जहां पर मन नहीं जा सकता । चक्षु इंद्रिय जिसको नहीं देख सकती और चक्षु इन्द्रिय को जो देखता है वही सनातन तत्व है, इदं रूप से जिसकी उपासना होती है वह सनातन परमात्मा नहीं है। कर्ण इन्द्रिय जिसको नहीं सुन सकती और इसके सुनने न सुनने दोनों को जो सुनता है। वाणी को मैं व्यक्त करता हूं, वाणी मुझ आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकती । मन को मैं जानता हूं। कोई ऐसा समय नहीं हैकि मन मुझ आत्मा से चोरी करके चला जाय । मन की चंचलता को जानता हूं, मन की स्थिरता को जानता हूं। उसके विक्षेप और लय को भी में आत्मा अनुभव करता हूं पर मन मुझ आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है। प्राण जिसको संचा- रित नहीं कर सकता । प्राण को जो संचारित करता है। वही स्व- स्वरूप अपना 'आप' है, इदम् रूप से जिसकी उपासना होती है वह ब्रम्ह नहीं है, वह परमात्मा नहीं है। वाणी करके, मन करके, चक्षु करके, प्राण करके तथा अन्य इन्द्रियों करके भी में आत्मा अग्राह्य हूं और मै स्वयं करके अग्राह्य हूं।। क्योंकि ग्रहण और त्याग तो उस बस्तु का किया जाता है। जो वस्तु अपने आप से भिक्ष होता है। 'में' जब अपना आप ही हैं, अपने आप से न में दूर हूं न अपने आप से निकट हूं।
दूर से दूर हूं मैं और निकट से निकट हूं। तो दूर से दूर कब हैं ? जब में आत्मा अपने आपको कुछ मान लेता हूं तो दूर से दूर हो जाता हूं और इतना दूर हो जाता हू कि जिसकी कोई सीमा नहीं और जब मान्यता हट जाती है। अपने ऊपर जो पर्दा है (मान्यता ही पर्दा है) तो इस मान्यता रूपी पर्दे को हटाने में ब्रम्हादिक भी समर्थ नहीं हैं। किसी और ने पर्दा डाला हो तो कोई निकाले । कोई और ढांका हो तो उस ढक्कन को कोई उठावे । जब अपने आप ही ढक्कन लगा लिया है तो कौन हटाए भैय्या ?
'सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा ।
यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ' ।८२।
(गौड पाद. कारि. अलातशा. प्र. मं. क्र. ।।८२।।)
भगवान आत्मा तो सुख पूर्वक ढांका जाता है। सुख पूर्वक छिपाया जाता है यह। मगर 'दुखं विव्रीयते सदा ।' और जब ढक्कन उघाड़ने का कोई समय आता है तो बड़ी कठिनता से वह ढक्कन है जो उघरता है । अपने आपको कुछ मान लिया ढक्कन बन गया। मानने में क्या देरी लगती है मगर वह मान्यता रूपी पर्दा जो पह गया उस पर्दे का उघड़ जाना सरल नहीं है यह ।
सुखमा ब्रियते ... …………….. … .. .... भगवानसौ ।
स्व-स्वरूप भगवान आत्मा पर सबसे पहला ढक्कन है- 'जीब भाव' बस ! यह पहला परदा है, और मान्यताएं तो बाद में आई
'जीवं कल्पयते पूर्व ततोभावान्पृथग्विधान ।
बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथाविद्यस्तथास्मृतिः ।
(गौड़ पा. कारि. वैतथ्य प्रकरण मंत्र क्रमांक ।१६।)
प्रश्न होता है- यह जीव आया कहाँ से ? इस जीव को पैदा किसने किया ? यह जीव भाव कब से आया ? यदि कहो कि-- में जब हूँ क्यों कि में न कहो, खाली जीव कहो, में न कहकर खालो जीव कहो तो जीव के आगे है आएगा। "जीव है"। हूँ नहीं आएगा । और हूं जो क्रिया है 'मै" की है न कि जीव की है। जीव हूं कहो या मैं जीव हूं कहो । एक ही बात है। मगर क्रिया से कर्ता का पता लगता है। व्यावहारिक जगत में देखो किसी व्यक्ति की क्रिया से ही उसके व्यक्तित्व का पता लगता है। किसी व्यक्ति की क्रिया से ही उसकी खासियत का पता लगता है कि कैसा है यह। जो 'हूँ' है, वह 'मैं' की क्रिया है। क्योंकि हूँ क्रिया जीव की नहीं है। फिर में करके जीव की सिद्धि है कि जीव करके, जीव की सिद्धि है ? तो फिर कौन कहता है ? कि में जीव हूँ। संसार में लोग कहते हैं कि मैं तो अपने आपको जीव मानता हूँ । तो भैय्या ! तुम अपने आपको जीव मानते हो तो तुम कौन हो? मानने वाले । 'मैं' अपने आपको जीव मानता हूँ जो ऐसा कहता है तो क्या वाकई दर असल; में जीव हूँ ? क्या सचमुच में जीव हूँ ? उससे पूछो तो वह कहेगा हाँ साहब में तो जीव मानता हूँ। तो अब उसका नाम मत लो, गंगाधर, रामप्रसाद । ओ जीव । कह कर पुकारो। उसका नाम मत लो और जीव नाम पुकारते से उसको गुस्सा न आवे, उसी मूड में रहे तत्र समझो कि हकीकत में यह जोव है और मत्थे पर सिकुड़न आ जाय तो समझो जीव नहीं है, भगवान है। कहाँ से प्रक्रिया सिद्धांत लगाओगे भला! यह भगवान की खोज है यह उसका पाखंड है कि जीव हूँ कहता है। महिला समाज अपने आपको स्त्री मानता है। अपने को डौका (पुरुष) कभी न कहेगी । तो किसी को कहो - ऐ डौंकी ? पचास गाली न सुनावें तो हमारा नुस्खा गलत। डौकी कहने में न चिढ़ें तब तौ डौकी हैं और चिढ़ जाएँ तो भगवान हैं। यही सुखमा ब्रीयते नित्यं।" यह तुमको समझाने की जरूरत नहीं कि तुम भगवान आत्मा हौं । यह सीजो हमारी प्रक्रिया। ये स्त्री कहके पुकारो ? अगर चिढ़ती है तो भगवानं हैं।
जीवं कल्पयते पूर्व………………………।
साक्षात् परमात्मा सबसे पहले अपने को जीव माना और कौन करेगा कल्पना । अरे भाई ! विकल्प का कोई न कोई आधार तो होना चाहिए । सोना न होगा तो आभूषण किसको मानोगे ? तो कोई न कोई चीज है। जीवं कल्पयते पूर्वं !
सबसे पहले जीव भाव की कल्पना होती है भगवान को फिर अलग-अलग जितने भाव हैं, पृथ्वी, जल, वायु अग्नि, आकाश, शब्द रूप, रस, स्पर्श, गंध, जागृत, स्वप्न, सूषुप्ति तीनों अवस्था में पंच कोष, तीन गुण ये बाद में होते हैं। " ततो भावान् पृथग्विधान् । " ये सर्व भाव पैदा हुए । लेकिन सबसे पहले इन विकल्पों का सबसे बड़ा भाई जीव । परमात्मा ही अपने आपको मानता है कि मैं संसारी जौंव हूँ। अगर इस कथन पर किसी को एतराज है तो शास्त्र प्रमाण तो है ही। यह कहता कौन है कि में जीव हूँ। यह कहने वाला कौन है ? अच्छा ! जीव का लक्षण पूछो फिर । तो जीव का क्या लक्षण है ? छोटा । छोटे से छोटा हो जीव (तुमने देखा है कभी कि सुन के कहते हो किसी से ?
जीव कल्पयते पूर्व …………………………… स्मृति ।
अपनी माया करके अपने आप ही मोहित हो रहा है।
स्वयमेव विमोहित :-
कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वभायया ।
स एव बुध्यते भेदानिति नेब्रास्तनिश्चयः ।"
(गौड़ पाद० कारि० वैतथ्य प्रकरण मंत्र क्रम ।।१२।।)
अपने आप करके अपने में अपने 'में' की ही कल्पना करता है। दूसरा कहाँ से आ जायगा। और फिर इन भेदों को जानता भी है। में ईश्वर नहीं हूँ, में तो जीव हूँ यह जो जीव भगवान का भेद है इसको जानता भी है। और, दूसरा कौन जानेगा । स एव बुद्धयते भेदान् । इन भेदों को स्वयं ही जानता भी है। इति वेद्वान्त निश्चयः। "और यह निश्चय सार्वभौम है। सुखमां क्रियते नित्य।"
"यस्य कस्य च धर्मस्य"
भगवान आत्मा को नाना प्रकार के धर्मों से लोग ढ़ाँकते है। • कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है। ढक्कन लग गया । ढांका तो सुखपूर्वक जाता है, मान लिया बँक गया । कितना सरल ढक्कन है। 'मैं' जीव हूँ। बँका तो सुखपूर्वक मगर जीव श्वाव का अभाव करने के लिए स्वयं ही जब चाहै, यह बात दूसरी है कि सन्त, महात्मा, गुरुजन उपदेश करते हैं, समझाते हैं। मगर स्वयं की इच्छा हो तब न, स्वयं की इच्छा, अपने को जानने की क़्यों नहीं होती ? इसलिए कि जब न जानता हो तब न, यह सहजान्नस्था का सत्संग है। सहजपद का विवेचन है यह। अपने आपको जानने की इच्छा क्यों नहीं होती, क्योंकि जानता है। इच्छा क्यों हो ? अब यहाँ सिद्धान्त, प्रक्रिया कुछ नहीं है भला ! अरे जानता है। क्या जानता है ? कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता । अरे यार ! जानना न जानना तो जीव का धर्म है ।
"हर्ष, विषाद, ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना।" इसलिए कुछ नहीं जानता । यही जानता है कि, अपने आपको कुछ नहीं जानता । इसलिए कि भगवान है। अरे यार ! जीव को जानने न जानने का विकल्य होता है कि भगवान को । जीव को न कि भगवान को । मस्त है फिर ! वाह ! और कैसा घुला-मिला है कि किसी को दिखता नहीं है कि देख सके ! क्योंकि अग्राह्य है वह । देख सके, जान सके । वाह । और ऐसा भी तो नहीं घुला- मिला है जैसे दूध और पानी । दूध और पानी का पता चल जाता है मगर दूध में दूध मिला है तो उसका क्या पता लगेगा भैय्या ! जो पदार्थ जैसा है उसमें उसो रूप से हूँ। किसकी ताकत है कि मुझ आत्मा का उसमें से पृथक्करण कर सके । जान सके । इसलिए में अग्रह्य हूँ। जी हाँ। वाह । हाँ। तो अपने आपको जानने की इच्छा क्यों नहीं होती क्योंकि में अपने आप से अज्ञात कब हूँ कि मुझ आत्मा को जानने की इच्छा हो । बंधन से छुटकारा पाने के लिए अपने आपको छुटकारा क्यों नहीं होती ? क्योंकि में बंधा होऊँ तब तो न । देखो, कमरे के अंदर पड़े हो और दरवाजा लगा हुआ है। सांकल लगा लिया है अंदर से लॉक कर लिया है और खर्राटे की नींद ले रहे हो क्योंकि उस ताले की चाबी मेरे पास है। घबराहट नहीं पैदा होती क्योंकि वह अपना बंधन लगाया हुआ है। अगर तुमको पता लग जाय कि किसी ने बाहर से सांकल लगा दिया है तो कहोगे - फिर टट्टी-पेशाच लगही तब फेर कैसे निकल बो दूसरे के बंधन लगाने में तो घबराहट होती है। पर जिस की कुंजी अपने पास है तो उसमें घबराहट को क्या बात । इसलिए भगवान को घबराहट नहीं होती खोल लेंगे और खोलता ही है ।
मृत्यु से क्यों भय लगता है? इसलिए कि कभी मरा नहीं । जो एक फर्लांग भी नहीं चलते और आज दस मील चलने का मौका लग जाय तो दिल में धड़कन पैदा हो जायगी क्योंकि आदत नहीं है। तो मरा तो कभी है ही नहीं। तो मरा कभी नहीं है। इसलिए कोई मरने का नाम लेता है तो घबराहट पैदा होती है। इसको सहजावस्था का सत्संग कहते हैं। जो चीज जैसी है उसको वैसी ही जान लेना इसका ही नाम बोध है। जो जैसा है उसको उसी प्रकार से जान लेना चाहिए । उस पर कलई करने की जरूरत न पड़े। ये बात ! क्यों ? जो जैसा है उसको वैसे ही जानना। इसका ही नाम बोध है तो मैं आत्मा जैसा हूँ उसको उसी प्रकार से जान लेना इसका ही नाम ज्ञान है। मैं आत्मा सत् हूँ, चित हूँ, आनन्द हूँ, कूटस्थ हूँ, अखंड हूँ, व्यापक हूँ, वगैरह-वगैरह ये तो सब ऊपर से चाल-चलन बनाना है। जो 'मैं' हूँ वह तो तुम जानते ही हो । एक दृष्टांत सुना है कभी । उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला है। उन्नाव जिले में एक मौजा है। किसी जमाने में वहाँ हम एक-एक महीने ठहर जाते थे । वहाँ एक मेजर साहब थे (अब तो नहीं रहे) उनके यहां में ठहरा करता था। साथ में चार पांच साधु भी रहे। एक दिन सुवह का वक्त था, मेजर साहब फौजी ड्रेस में वहीं हमसे कुछ दूरी पर चहल कदमी कर रहे थे, कि वे हमको अकेले बैठे देख कहने लगे - स्वामीजी ! हमने कहा- हाँ मेजर साहब ! उनने कहा- आज तुम्हारे चेला वेला कहाँ गये हैं ? दिख नहीं रहे हैं?
हमने कहा- मेजर साहब ! वे सब भजन में बैठे हैं। तब वे कहने लगे कि भजन में बैठे हैं कि चाल चलन बना रहे हैं ?
हमने पूछा- चाल चलन बया है मेजर साहब ?
वे कहने लगे - हमारी फौज में एक सिपाही था, उसका नाम - था महेश सिंग । वह भी ठाकुर था। रोज उसकी शिकायत हमारे पास आया करे । कभी किसी की बाड़ी से फल, सब्जी तोड़कर ले आवे, कभी किसी महिला की कलाई से घड़ी छीन ले आदि । एक दिन हमने क्या देखा, सुबह के वक्त में टहल रहा था ठण्ड खूब पड़ रही थी, कड़ाके की। बरामदे में एक कोने में कोई रामनामी दुपट्टा ओढ़े खटर खटर माला फेर रहा है। मैंने पूछा- कौन आय गया है हमार फौज में ? रोज दो घंटा माला फेरत है, तो सिपाहियों ने कहा- वही महेशवा है सरकार ! जिसकी आपके पास रोज शिकायत आती है। तो हम बूट पहने थे, पीछे से जाकर उसे एक लात मारा उसकी पीठ पर और हमने कहा, हमारे पास रोज तेरी शिकायत आती है और तू यहाँ बैठकर पाखण्ड कर रहा है, राम नामी दुपट्टा ओढ़े माला फेर रहा है। वह भी ठाकुर था, और हम भी ठाकुर, इसलिये बूट पहने हुए उसे लात से मारा, यदि ब्राह्मण होता तो नहीं मारते ।
लात के लगते ही वह दुपट्टा फेंककर माला वहीं रख दिया और इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है और फिर झट दोनों हाथों से हमारे पैरों को पकड़ लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि सरकार ! जो मैं हूं वह तो तुम जानते ही हो यह तो ऊपर से दुनियाँ दिखाने के लिये चाल चलन बनाउथ हैं, ऐसा कह झट वहाँ से वह चुपचाप चला गया ! तो, स्वामी जी ! चेला लोग ऐसे चाल चलन तो नहीं बना रहे हैं ?
हमने कहा- नहीं मेजर साहब ! वे भजन में बैठे हैं। भैय्या ! उस दिन से हमने इसको अपने परमार्थ में घटा लिया तो जो में परमात्मा हूँ और जैसा हूँ वह तुम जानते ही हो और जो बात रह गई सत् हूँ, चित् हूँ आनंद हूँ यह तो ऊपर से चाल-चलन बनाना है।
"नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वताभिधा ।
यत्न वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते" ॥६०॥
(गौड़ पा० कारि० अलाल शा० प्रक० मंत्रसं० ॥६०॥)
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।
यग्दत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम् ॥
(गीता - अ० १५ श्लोक ६)
वाणी जहाँ पहुँच नहीं सकती तो क्या कहा जा सकता है कि में परमात्मा ऐसा हूँ। तो जो मैं हूँ वह तो तुम जानते ही हो । ऊपर से जो यह सुन रहे हो वह चाल चलन बनाना है। मगर वस्तुतः नहीं है ज्ञात किसी को इसलिए श्रुतियाँ भी नेति-नेति कह- कर भाग जाती हैं क्योंकि नजदीक जाय तो छुआ जाय। जहाँ भगवान को छुआ तो भगवान हो गया। दूर खड़े होकर हकीकत का बयान किया नहीं जा सकता। इसलिए मैं अग्राह्य हूँ। यानी दूर खड़े होकर मैं आत्मा की वास्तविकता को मैं आत्मा की सचाई को हैं वह दूर से नहीं जाना जाता जो कुछ कहें चाल चलन बनाना है और नजदीक जाते हैं तो छुआ गए । भगवान हो जाता है। तो क्या हकीकत है। क्या सचाई है। इसलिए साहब जो में हूँ। वो तो तुम जनते ही हो। इसलिए में अग्राह्य हूँ और फिर तारीफ यह है कि दूसरा क्या कहेगा। में जब खुद ही अपने आप से दूर होकर क्या मैं अपने आपका बयान कर सकता हूँ। अपने आप से दूर होना क्या है ? अपने आप को जीव मान लिया । न तो जीव रूप से अपने आपका कथन कर सकूं और न आत्मा रूप से अपने आपका कथन कर सकूं इसलिए कि मैं अग्राह्य हूँ ।
"स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर्दुरव्ययानुक्रमणो निरूव्यते ।
ह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयोह्येष मिनत्तिमेमतिम् ।।१३।।
(श्रीमद्भागवत् सप्तम स्कंध अध्या० ५ श्लो १३)
ब्रह्मादिक भी निश्चय करने में समर्थ नहीं है कहते हैं। बड़ी अच्छी युक्ति है। अगर दूर होकर के कहूँ भगवान से अलग होकर भगवान को बताना चाहूँ तो नहीं बता सकता। दूर होकर कहने में नहीं वनता और नजदीक जाते हो तो छुआ जाते हो । हाँ, इतना ही कहता है- जो कुछ में हूँ सब तुम जानते ही हो । क्या ? अगर जो मैं हूँ तुम जानते ही हो तो तुम अगर मुझ से दूर हो तो तुम जानते ही हो। यह कहते न बनेगा। वह 'मैं' आत्मा के लिए कहा जा रहा है- कि साहब तुम तो जानते ही हो। बाकी जो कुछ भी है कर्मकाण्ड उपासना काण्ड ये सब चाल-चलन बनाना है भैय्या । ऊपर से चाल-चलन बनाना है। हकीकत तो जो है वह अग्राह्य है। इसके ग्रहण में कोई आजतक समर्थ हुआ ही नहीं इसलिए श्रुति सच समझकर कहती है "अग्राह्यम्" में आत्मा अग्राह्य हूँ क्योंकि श्रुति बेवकूफ थोड़ी है वह समझती है। श्रुति कहती है कि अगर मै दूर होकर कहूँ तो अग्राह्य और नजदीक होकर कहूँ तो वही हो जाऊँगी तो अग्राह्य । हाँ जी, ब्रह्मादिक मुझ आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है तो यह जीव भला कैसे जान सकता है इसलिए जीव को भगवान के जानने में कोई अधिकार नही है।
हां अरे ! चौपाई क्या भूल गए हो ?
'जानत तुमहिं तुमहिं होइ जाई ।'
यह बाल्मीकि जी कहते हैं ।
तुम्हरी कृपा तुमहिं रघुनंदन। जानहिं भगत-भगत उर चंदन ।'
तो भैय्या ! आज तक जिसने जाना वह यह बताने को नहीं आया कि भगवान को मैंने इस प्रकार जाना । वापस आकर किसी ने कहा हो भगवान ऐसा है, भगवान इस प्रकार है। मैंने जाना है आज दिन तक किसी ने कहा नहीं। क्योंकि कहेगा क्या ? भगवान को जानकर अगर भगवान से भिन्न होय तब तो कहे कि भगवान ऐसा है । जब जानत तुमहि । जब छू लेने पर भगवान ही हो गया तो किससे कहें । इन सब बातों को मद्दे नज़र रखते हुए 'मैं' आत्मा अग्राह्य हूं । अरे भाई में कुछ कहूंगा तो वाणी द्वारा ही तो कहूंगा। तो अगर में कहूं मैं ऐसा हूं तो 'में' नहीं और कहो कि जैसा हूं तो 'वाणी' कहां' तो है न मुसीबत साफ तौर से । इसलिए 'में' अग्राह्य हूँ यह अग्राह्य का विवेचन है। यदि में कहूं कि ऐसा हूं तो "यतो वाचो निवर्तन्ते" यह श्रुति कहां जायेगी । वाणी जहां से वापस आ जाती है मन जहां जा नहीं सकता और यदि में कहूं कि 'मैं' ऐसा हूं तो वाणी पैदा होती है और जैसा हूं में वाणी 'मैं'हो जाती है। दृष्टि 'में' हो जाती है। कर्ण इन्द्रिय में हो जाती है मन-बुद्धि चित्त, अहंकार सब 'मैं' हो जाते हैं। सब छुआ गए। ऊं । हां, जी। क्योंकि 'में' अग्राह्य हूं। मैं अग्राह्य हूं 'मैं' अग्राह्य हूं।
अब यहां एक प्रश्न होता है-कि भगवान आत्मा को जानने के लिए जो कुछ भी किया जाता है कर्मकाण्ड है, उपासना है, भजन, है पूजा है, आरती है, योग है, ध्यान है, धारणा है, और समाधि है यह भगवान को जानने का साधन नहीं है। 'भगवान' को जानने का जो अधिकार है, उसे प्राप्त करने के साघन हैं, ये सब । अधिकार प्राप्त हो जाता है भगवान प्राप्त करने के लिए । क्योंकि इनकी भी तो मर्यादा रखनी है। इन सत्रों से, पूजा से, पाठ से, नाम स्मरण से जो कुछ भी किया जाता है चाहे जानकर करो या अनजान में करो अधिकार प्राप्त होता है। 'बैंक ग्राउण्ड' बनता है। और जब भगवान श्रीराम लक्ष्मण से कहते हैं-
'आदौ स्ववर्णाश्रम र्वाणताः क्रियाः,
कृत्वा समासादित शुद्ध मानसः ।
समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधनः,
समाश्रयेत्सद्गुरु मात्मलब्धये' ।७।
(अध्या. रामा. उ. काण्ड ५ पंचम सर्ग श्लोक ।७।)
अपने-अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करके अंतःकरण पवित्र करे । इसके बाद क्या करें, इसको छोड़ दें। भगवान आल को जानने के लिए सद्गुरु की शरण में जाय । अध्यात्म रामाय की रामगीता का सातवाँ श्लोक है । आत्मा की उपलब्धि के लि आत्मा को जानने के लिए जो है. सद्गुरु की शरण में जाय। इसमें अधिकार प्राप्त का साधन भी हो गया और जब अधिकार प्राप्त हो जाय तो गुरु की शरण में सर्पित हो जाय । अपना वा मिटा दे तो इसलिए यह जानकर कि भगवान आत्मा अग्राह्य है। ऊपर से जो कुछ करना है चाल चलन बनाना है। ऐसा न हो इसको सुनकर गलत अर्थ लगालें अपने हृदय में तो दोनों ओर गए पाँडे, हलुवा मिली न मांड़े । महारानी प्रकृति ने 'मुक्त आचार्य के आसन पर बिठाया है तो सबकी मर्यादा को लेकर विवेचन होता है। किसी का यहां खण्डन नहीं होता। क्या करना बाहिए, कब तक करना चाहिए, इसको करने का क्या फल है ? यह हम बताते हैं। यहां तो खण्डन का भी खण्डन नहीं होता ।
'उमा जे राम चरण रत, विगत काममद क्रोध,
निज प्रभुमय देहि जगत केहिसन कर्राह विरोध ।'
तो भैया ! यहां खण्डन नहीं होता। अच्छा, सगुण ब्रम्ह की उपासना कब तक करनी चाहिए यह भी सुनो- भगवान राम ने रहा है लक्ष्मण से-
'यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकं, तावन्मदाराधनतत्परो भवेत् ।'
श्रद्धालुरत्यूजित भक्ति लक्षणो, यस्तस्य दृश्योऽहमनिशं हृदि ।५८।'
(अध्या. रामा. उ. काण्ड पंचम सर्ग श्लोक सं. ।५८।)
हे भाई लक्ष्मण ! जब तक सारा प्रपंच तृण से आदि ब्रम्हा पर्यंत आप सहित अपना स्वरूप न दिखाई देने लगे तबतक मेरी आरा- बना करे। सबका कोर्स है। ऐसा थोड़े ही है कि जिंदगी भर नही करता रहे। शास्त्रों का मंथन किया जाय विलोडन किया जाय, विचार किया जाय तो यह सब बात निकलती है। सांगो-पांग विवे- चन होता है इसलिए यहाँ सब आते हैं। हिन्दू-मुसलमान, ईसाई, रंन, बौद्ध, आस्तिक और नास्तिक सब आते हैं। सबको संतोष निहाता है। जिसको अधिकार प्राप्त है वे तो हैं ही, जिनको अधिकार राप्त नहीं है उन्हें भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर ऐसा तो भी है यदि सगुण भगवान की आराधना नहीं किया तो जहां पर न्ह विद्या का विवेचन होता है और पहुंच गया वहां पर इसको अधिकार भी मिल जाता है। सब हो गया। कुछ भी नहीं करना धरना पड़ता । ब्रम्हा विद्या के श्रवण से अंतःकरण की शुद्धि होती है, करोड़ौ जन्मों के पातक नष्ट हो जाते हैं। मल का नाशक श्रवण विक्षेप का नाशक मनन, आवरण का नाशक निदिध्यासन है। बाद में तो सद्गुरु माश्रयेत् । तो भैय्या में आत्मा हूं क्योंकि मन द्वारा मनन् न हो, चित्त द्वारा चिंतन न हों । बुद्धि द्वारा निश्चय नहीं । तो प्रश्न होता है कि किस प्रकार जाना जाय । तो मन मनन करते- करते जहां पर अपन हो जाता है। चित्त चिन्तन करते-करते जिस अवस्था में चित हो जाय । बुद्धि जहां पर खो जाती है और बुद्धि का निश्चय धर्म खतम हो जाता है। वही तो मैं आत्मा हूं । परनु मन-बुद्धि-चित्त करके मैं अग्राह्य हूं। इन सब करके में अग्राह्य हूं। तो
'नान्तः प्रज्ञं न वहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञान घनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम ।
अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यम लक्षणम चिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म
प्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः' ।७।
(गौ. पा. कारि. आगम प्रकरण मंत्र सं. ।७।)
जब में अग्राह्य हूं तो अग्राह्म होने के कारण मैं अव्यवहार्य हूँ व्यवहार में 'मैं' आत्मा नहीं आता । इसलिए अव्यवहार्य हूं कि म आत्मा में व्यवहार नाम की चीज नहीं है। अरे ! व्यवहार है ही नहीं व्यवहार का मतलब - न मुझ आत्मा की दृष्टि व्यवहार कर सके कर्ण इन्द्रिय व्यवहार कर सके न जिव्हा व्यवहार कर सके । जि इन्द्रिय का जो धर्म है, जैसे आंख का देखना धर्म है, वाणी बोलना धर्म है । ये इन्द्रियों के व्यापार हैं अथवा इन्द्रियो के व्यत्र- हार हैं। तो इन व्यबहारों करके 'में' अव्यवहार्य हूं। दूसरी चीज यह है कि मुझ आत्म-देश में व्यवहार है ही नहीं। मुझ आत्मा के लिए कोई व्यवहार नहीं । 'मे' आत्मा से व्यवहार नहीं और 'मुझ' आत्म-देश में किसी किस्म व्यवहार नहीं। मुझ आत्मा के लिए व्यबहार नहीं 'मैं' 'आत्मा' स्वयं व्यवहार रूप नहीं और मुझ आत्म देश में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं अनभव करा । कल भी इस पर थोडी रोशनी डाली गई थी । समझाया गया था। जिस समय 'मे' आत्मा यानी शब्द, रूप, रस गंध और स्पर्श इत्यादि विषयों में - विषय का अनुभव करता हूं तो किसी विषय के अनुभव काल में 'कर्त्तानुभूति', कर्मानुभूति, क्रियानुभूति आदि तीनो अनुभू- तियो की अनुभूति नहीं होती । फिर सुनो शब्दादिक विषयों में से किसी भी विषय के अनुभव काल में तोनों चीजे रहेंगी ही नहीं । 'अनुभव' करना क्रिया है और जिस चीज का अनुभव किया जाय वह कर्म है और अनुभव करने वाला कर्त्ता है तो किसी भी विषय के अनुभव काल में किसी की अनुभूति नहीं होती और अगर होती है तो में अव्यहार्य नहीं। जी हां ! किसी भी विषय के अनुभवकाल में किसी भी दृश्य के दर्शनकाल में, किसी भी रस के ग्रहण काल में, किसी भी पदार्थ के स्पर्शकाल में कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों का अभाव रहता है । इसलिए इस अनुभूति को लेकर महारानी श्रुति कहती है- 'अव्यवहार्यम् ।' एक बात है कि किसी भो विषय के अनुभव काल में कर्त्ता, कर्म, क्रिया तीनों की अनुभूतियो का अभाव रहता है तो इसकी अनुभूति तो अनुभूति देश ही होगी। किसी भी विषय के अनुभव काल में कर्त्ता, कर्म, क्रिया तीनों की अनुभूतियो का अभाव रहता है- इसका जो 'अनुभव' वह 'अनुभव देश' में हो होगा। 'मैं' देश में । बुद्धि तो यहां तक कहती है कि में अनुभव करती हूं और यह फलाँ विषय है। मगर ऐन अनुभव-काल में बुद्धि भी खो जाती है, मन खो जाता है, चित्त खो जाता है। इनका एक का भी पता नहीं रहता तो कत्र्ता, कर्म, क्रिया तीनों का अभाव रहता है इसलिए श्रुति मुझ आत्मा को अव्यवहार्य कहती है ।
अब बारह बज रहे हैं, मध्यावकाश के बाद
दो बजे से प्रवचन पुनः प्रारम्भ होगा ।
** *
समय- २ बजे से ४ बजे तक
स्वरूप जो आत्मा 'मैं' नाम से प्रसिद्ध है, भगवान आत्मा के विशेषणों की व्याख्या की जा रही है।
नान्तः प्रज्ञम् ....
उस वक्त अव्यवहार का विवेचन हो रहा था ।
नान्तः प्रज्ञं ….
न 'मैं' आत्मा भीत्तर को जानता हूं न 'मैं' बाहर को जानता हूं। न 'मैं' प्राज्ञ हूं न अप्राज्ञ हूं। अदृष्टम 'मैं' भगवान आत्मा अदृष्ट हूं। अदृष्ट का विवेचन हो चुका है 'अग्राह्यम्' इन्द्रियों करके अग्राह्य हूं । मुझ आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता ।
'अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः ।
चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव बालिशः ।' ।८३।
कोट्यश्चतस्त्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृतः ।
भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक् ॥' ।८४।।
(गौ. पा. कारि. अलात शांति प्रकरण मं. सं. ।८३-८४।)
कोई कहता है कि ईश्वर 'है', परमात्मा है। कोई कहता है, ईश्वर 'नहीं है।' कोई कहता 'है' और 'नहीं है' और कोई कहता है 'नहीं है-नहीं है' । जो कहता है-ईश्वर 'है' वह मूर्ख है, जो कहता है- 'नहीं' 'है' वह भी मूर्ख है। जो कहता है- "है और नहीं है" वह भी मूर्ख है और जो कहता है- 'नहीं है- नहीं है', वह महामूर्ख है कहो । अलात् शाँति प्रकरण की कारिका है यह। ये चारों कोटियाँ भगवान 'आत्मा' को ढांकने की कोशिश तो करती हैं पर ये चारों भगवान आत्मा का स्पर्श तक नहीं कर सकतीं ऐसा जो जानता है वह सबको देखता है। ऐसा जो देखता है वही स्व-स्वरूप भगवान आत्मा को जानता है। वही भगवान स्व-स्वरूप आत्मा को देखता है 'अदृष्ट' कोई कहता है कि भगवान है। ठीक है। जो कहता है, परमात्मा 'है' उसको मूर्ख क्यों कहा गया ?
जो कहता है-'है'। तो इसको कौन जानता है। प्रमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध कौन करता है? 'मैं'। यदि आज कोई भी विरोधी तुम्हारे सामने आकर कहे कि क्योंजी ! परमात्मा 'है' इसका क्या प्रमाण है? उस वक्त क्या तुम पोथी-पत्रा दिखाओगे ? उपनिषद्, भागवत्, पुराण आदि से भगवान आत्मा का अस्तित्व मिद्ध नहीं होता। ये तो आस्तिकों के ग्रंथ हैं। जो इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए तो ये ग्रंथ प्रमाणित हैं और जिनका परमात्मा के अस्तित्व पर ही सन्देह है, तो ये ग्रंथ प्रमाणित नहीं होते । उनके सामने इन ग्रंथों की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए । वे कहते हैं, कि तुमने अपने घर में लिख लिया होगा। परमात्मा के अस्तित्व में क्या प्रमाण हैं ? परमात्मा के अस्तित्व में यही प्रमाण है कि 'मैं' 'हूं' इसलिए परमात्मा भी है और यदि में नहीं तो परमात्मा भी नहीं । परमात्मा है इसको जानता कौन है ? इसका साक्षी कौन है ? यदि में न होऊंगा तो इसका प्रमाता कौन होगा कि परमात्मा 'है' । कोई कहता है कि परमात्मा 'नहीं है' तो जिस करके 'परमात्मा है' इसको सिद्धि होती है उसी करके परमात्मा 'नहीं है' की भी सिद्धि होती है तो नानाभाव का सिद्ध करने वाला तो 'मैं' ही हूं और परमात्मा-'है' और 'नहीं है'- इसकी भी सिद्धि में ही करता हूं और परमात्मा 'नहीं है- नहीं है' की भी सिद्धि में ही करता हूं परन्तु मुझ 'आत्मा' को अस्तिभाव, नास्तिभाव, अस्ति-नास्तिभाव और नास्ति-नास्ति- भाव चारों कोटियाँ स्पर्श करने में समर्थ नहीं है। यह अग्राहा का रूप है ।
परमात्मा नहीं है असद भावना है। विपरीत भाबना जीवात्मा परमात्मा दोनों भिन्न-भिन्न हैं। ईश्वर-सर्वज्ञ, है, जीव-अल्पज्ञ है। संभावना-शायद ऐसा ही हो। असंभावना- ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्हीं चारों भावनाओं के मूलोच्छेद करने के लिए वेदों के चारों
तत्वतः वय हैं। अहं ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम् ।। माता पार्वती के हृदय में असम्भावना पैदा हुई थी। जा तनय तो ब्रह्म किमि, नारि बिरहमति मोरि जब तत्त्व का बोध भगवान शंकर से तव माता जी कहती हैं---
भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति । दारुण असम्भावना बीती ।''
क्योंकि 'मैं' आत्मा सर्व करके अग्राह्य हूँ। कोई स्पर्श नहीं सकता तो अग्राह्य हूँ, अव्यवहार्य हूँ। व्यवहार में में आत्मा आता क्योंकि व्यवहार होता है प्रपंच में। और इन्द्रियाँ भी व का ही व्यवहार करती हैं। मन प्रपंच का व्यवहार करता है कि मुझ 'आत्मा' का और इन्द्रियाँ स्वयं प्रपंच हैं। मतलब यह है मुझ आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सब प्रपंच है। इन्द्रियाँ वयं प्रपंच हैं और प्रपंच का ही व्यवहार करती हैं न कि मुझ आत्मा का । इसलिए मैं अव्यवहार्य हूँ। मुझ आत्म देश में--
"न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥३२॥"
(गौ० पा० कारि० वैतथ्य प्रकरण मं० सं० ॥३२॥)
न निरोध है, न उत्पत्ति है, न पालन है न संहार है। में गमा परमार्थ स्वरूप हूँ। परमार्थ स्वरूप मुझे आत्मा में व्यवहार होने के कारण में अव्यवहार्य हैं। प्रपंच का अभाव तो कर दिया। त्रि का बाध तो पहले ही मंत्र में हो चुका । "
ओमित्येदक्षरी मिद्रꣲ᳭ सर्वम् ।
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न .....परमोर्थता । "
इस कारिका में न उत्पत्ति है न पालन है, न संहार है। जब
प्रपंच की उत्पत्ति नहीं तो फिर प्रपंच का पालन नहीं और जब प्रपंच की उत्पत्ति और पालन नहीं तो प्रपंच का संहार भी नहीं जब प्रपंच की उत्पत्ति नहीं तो फिर उत्पत्तिकर्त्ता गए पालन नहीं तो भर्ता गए, उत्पत्ति और पालन नहीं तो हर्ता भी गए। यह परमार्थ है।
यही उत्तम सत्य है कि किसी बीज की उत्पत्ति हुई ही नहीं कोई भला सिद्ध कर तो कर दे ।
"स्वतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते ।"
न तो प्रपंच स्वय पैदा होता है न इसे और कोई पंदा करत है । प्रपच स्वयं पैदा नहीं होता । क्योंकि यदि प्रपंच की उत्पति मानते हो तो प्रपच पैदा होने के पहले उसका क्या रूप था ? भा रूप था कि अभाव रूप था कि भावाभाव रूप था। तो प्रपच अपने उत्पत्ति के पहले सत्य था- तो श्रीमान् जी, सत्य की तो उत्पत्ति ह नहीं होती । जो कालातीत हो उसे सत्य कहते हैं जगत प्रपन उत्पत्ति के पहले सत्य था तो सत्य मानकर उत्पत्ति सिद्ध नहीं हाती असत्य कहो तो असत्य बन्ध्या पुत्रवत् होता है इसलिए जब था नहीं तो पैदा क्या होगा । उसकी उत्पत्ति कैसे होगी । सत्य मान तो उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, असत्य मानों तो उत्पत्ति सिद्ध नह होती । सत्या सत्य कहो तो इसका उत्पन्न होना सिद्ध नहीं होत न तो जगत प्रपंच स्वयं पैदा होता है न इसे कोई पैदा करता है यदि कहो - अगर पैदा नहीं हुआ तो यह प्रपंच परमात्मा से अ है। तो कहते है यह भी नहीं बनता क्योंकि जगत का कत्र्ता परमात्मा को माना जाय तो जो परमात्मा जगत का कर्ता है जन्मा है कि अजन्मा ? अगर जन्मा मानोगे तो परमात्मा सिद्ध होता । परमात्मा सत्य सनातन कहा जाता है। उसे अजन्मा कहो को श्रीमान जी किसी का जन्म सिद्ध नही होता। इसलिए परमात्मा व भी जगत की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। कोई पदार्थ न स्वयं बंदा हुआ न किसी ने पैदा किया। जब प्रपंच हो तब न प्रपंच का व्यवहार हो इसलिए में आत्मा अव्यवहार्य हूँ। और जब उत्पत्ति नहीं तो पालन किसका । और पालन नहीं तो संहार किसका । नीता स्मृति आई हैं- पंन्द्रहवें अध्याय में कहते हैं-
न रूप मस्येह तथोपलम्यते, नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा।"
(गीता अध्या० १५ श्लोक ३)
कहते हैं कि- आदि में उत्पत्ति, प्रतिष्ठा में पालन और अन्त में संहार । यह अव्यवहार्य की व्याख्या है। कहते हैं कि संसार का जंसा रूप देखने में आता है वैसा यह अपने मूल भाग में नहीं मिलता। इसलिए न इसकी उत्पत्ति है न पालन है न संहार है। यादि है न मध्य है न अन्त है। न रूप मस्येह ... ... ... ।
न आदि है, न मध्य है न अन्त है। न उत्पत्ति है न पालन है संहार है। तो उत्पत्ति रहित है। तो फिर क्या है यह ? मुझ मात्मा का भी तो उत्पत्ति पालन और संहार नहीं हैं। तो यह विशेषण प्रपंच का है कि मुझे आत्मा का है ? मुझ आत्मा का है।
'न रूप मध्येह तथोप लम्यते ......... संप्रेतिष्ठा ।'
कहते हैं न परमात्मा आदि, मध्य और अंत से रहित है। तो सार भी तो आदि, मध्य और अंत से रहित है। जैसे मुझ आत्मा उत्पत्ति नहीं, मुझ आत्मा का पालन नहीं, मुझ आत्मा का संहार हीं। क्योंकि अधिष्ठान में जो अध्यस्त पदार्थ होता है वह अधिप्टान के अनुरूप ही होता है । अधिष्ठान स्वरूप ही होता है। अधिष्ठान जो लकड़ी है और इस अधिष्ठान लकड़ी में डण्डा अध्वस्त है, तो जो रंग जो वर्ण लकड़ी का वही रंग वहीं वर्णं डण्डा का। तो इसी तरह जो लक्षण मैं 'आत्मा' का वही लक्षण प्रपंच का ।
"उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादजंऽ सर्व मुदाहृतम् ।
न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ।। "
(गौड षा० कारि० अलात शां० प्र० मंत्र ॥३८)
प्रपंच की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती इसलिए प्रपंच 'अज' और जो 'अज' है वह 'मैं' हूँ। संसार तो एक फर्जी नाम है। कल्पना करली । व्यवहार कहा जाता तो है पर जब प्रपंच हो तब व्यवहार हो । अरे ! जब प्रपंच बन्ध्या पुत्रवत् है, है ही नहीं, भैया फिर "अव्यवहार्यम्" में आत्मा अव्यवहार्य हूँ। व्यवहार लेश ही नहीं है। "न रूप मस्येह ।"
फिर यह कहो यदि यह संसार प्रपंच पैदा हुआ होता तो इस जन्म कुडली अवश्य होती परन्तु यह संसार कब बना ? किन बनाया ? कैसे बना ? इसका तो आज दिन तक किसी ने पता लगा पाया । इसके जन्म संवत् का भी पत्ता नहीं इसलिये सर अनादि है। अनादि होने के कारण 'मैं' हूँ । अनादि होने के कारण पालन का अभाव है, तो कर्त्ता, भर्ता और हर्ता इन तीनों का अभाव है। फिर अभाव में व्यवहार कहाँ इसलिए 'मैं' आ अव्यवहार्य हूँ ।
"अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा''
(गीता-१५ वां अ.)
देखो भगवान श्रीकृष्ण ने ससार का नाम दिया है अश्वत्थ । भैय्या- अश्वत्थ तो कहते हैं संस्कृत में पीपल के वृक्ष को । अ = नहीं । स्व = प्रातः । स्थ स्थिर । रात्रि के अंधेरे में तो रहे और प्रकाश होने पर सबेरे न रहे उसको कहते हैं अश्वत्थ ।
अज्ञान के अंधेरे में तो ससार है और ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर नहीं रहता । इसलिए भगवान ने संसार का नाम अश्वत्थ खखा । क्या बारह बजे दिन में रज्जू में सर्प दिखता है ? रात में हो दिखता है। और जहाँ रोशनी आयी तो उसका अभाव है। अच्छा, अज्ञान किस चीज का । अरे, रज्जू के ही अज्ञान से सर्प न होते हुए अंधकार के कारण सत्य सा भासता है। किस चीज का अज्ञान ? स्वरूप आत्मा का । अरे ! स्वरूप आत्मा के अज्ञान से ही यह संसार प्रपंच सत्य सा भास रहा है। वास्तव में है नहीं ।
न रूप मस्येह …………………….छित्त्वा :
भगवान कहते हैं कि और जो इसकी जड़ है संसार वृक्ष की जो जड़ है बड़ी मजबूत और बड़ी गहराई में गई हुई है। तो फिर संसार की जड़ काटें कैसे ? किस तरह इस जड़ को उखाड़ी जाय ? असंग शस्त्र करके । असंगोऽयमपुरुषः । असंग का मोटा 1 अयं है तो यही कि जिसको किसी की संगत न हो। तो मैं जो आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का संग किसी में है ही नहीं। अब यह प्रश्न होता है- कि संसार का संग तो आत्मा का है ही ? अरे ! • होय तब तो संग करे आत्मा का । अरे ! मुझ आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं तो संग किसका । तो इस संसार की सजबूत जड़ है उसको किस शस्त्र से काटे। असंग शस्त्र से । असंग बया है ? 'बात्मा' और कहते हैं कि यह जो असंग शस्त्र है इतना पैना है कि दृढ असंग शम्त्र करके काटे इस संसार के जड़ को । रज्जू से यदि सर्प भिन्न है तो उस सर्प का नाश करने के लिए कोई न कोई दूसरा उपचार हो सकता है। अरे ! जब रज्जू ही सर्प है तो फिर उस सर्प को काटने के लिए रज्जू ही शस्त्र है। उसी तरह संसार प्रपंच यदि मुझ आत्मा से सर्वथा भिन्न है तब तो संसार के नाश का दूसरा उपचार हो सकता है और जब में ही प्रपंच हूँ तो ''मैं'' आत्मा ही उस प्रपंच के नाश का शस्त्र हूँ। इसलिए असंगोऽयम-पुरुषः ।
अज्ञान रहित, स्वप्न रहित, नाम रूप से रहित, स्वयं प्रकाश। सर्व का ज्ञाता । जब hat F आत्मा ऐसा हूँ तो फिर कोई उपचार नहीं । तो 'न रूप मस्येह तथोपलभ्यते !
रज्जू ही है, जिसको सर्प कहते हैं। सर्प तीन काल में नहीं है। तो भैया सारे व्यवहार होते हैं प्रपंच में, और प्रपंच तीन काल में है नही, तो व्यवहार की सिद्धि कहाँ और व्यवहार की सिद्धि नहीं तो मैं आत्मा अव्यवहार्य हूँ ।
देखो - इस देह को ले लो। यह देह अपनी उत्पत्ति के पहले सत्य था कि असत्य था, कि सत्या सत्य था । सत्य कहो तो उत्पत्ति नहीं । असत्य कहो तो उत्पत्ति नहीं । सत्या सत्य कहो तो उत्पन्न नहीं हुआ । तो अनुत्पन्न होने के कारण 'अजम्' ।
उत्पादस्या ………………………. कथंचन ।
उत्पत्ति की असिद्धि होने के कारण "इदं प्रपंच अजम् ।" सब अजम् है। यही संसार जड़ काटने का शस्त्र है। देखो - अपने आपको आत्मा जानकर (जीव मानकर नहीं) ध्यान में बैठो और अगर भीतर विचार, कल्पना, संकल्प, विकल्प जो भी दृश्य तुम्हारे सामने आए, क्योकि मैं आत्मा तो जानता ही हूँ । विचार उठते है तो मैं जानता हूँ। तो जब कोई भीतर दिखाई पड़े दृश्य, उस दृश्य को काटने के लिए उस प्रपंच को नष्ट करने के लिए कौन सा शस्त्र हाथ में पकड़े रहना चाहिए। अरे ! 'अहम्' । जब विचार पैदा हो वह कल्पना हटाई जा नहीं सकती । कुछ मत करो । जब कोई चीज़ पैदा हो अंदर 'अहम्' । मैं का डंडा लगाओ। जहाँ तुमने यह भावना किया तो में का डण्डा लगते ही न तो तुमको विचार दिखेगा न संकल्प-विकल्प दिखेंगे । न कोई विकार दिखेगा। यह हथियार पकड़ लो । यह हथियार बिना लाइसेंस का है। यह हथियार सब के पास है और बिना लाइसेंस का है। इसमें कोई पूछने वाला नहीं है कि लाइसेंस दिखाओ । यह विश्व विजयी हथियार है। इस हथियार से सारा प्रपंच ही खत्म हो जाता है। और इस हथियार को लेकर कहीं भी जा सकते हो । पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। कहीं जाओ चाहे घर में रहो । चौबीस घंटे यह हथियार लटकाए रहो । काम चेष्टा, क्रोध चेष्टा, लोभ चेष्टा ये बड़े प्रबल शत्रु हैं। सबके लिए बस एकही हथियार है। इन्द्र का बज्ज्र भले कुंठित हो जाय । मगर यह कुंठित नहीं हो सकता । प्रपंच के अस्तित्व से भय है। या अस्तित्व से भय है ? प्रपंच है। जगत प्रपंच है तो प्रपंच से भय है। है देश में प्रपंच है कि प्रपंच देश में प्रपंच है ? डण्डा देश में डण्डा है कि लकड़ी देश में डण्डा है। 'है' देश में प्रपंच है कि प्रपंच देश में प्रपंच है ? प्रपंच देश में। जहाँ तुमने डण्डा मारा 'मैं' हूँ तो में आत्म देश में तो प्रपंच है ही नहीं तो फिर भैया -- चला गया । मगर इस हथियार का इस्तेमाल उसी समय करो जब तुमको उस चीज से भय लगे। हरेक पर इसे न मारो। देवराज इन्द्र उस समय वज्त्र का प्रयोग करता है कि जब वह समझ जाता है कि में गया अब नहीं बच्गा । इन्द्र का मारा हुआ नहीं बचता । तो 'मैं हूँ' इसका उपयोग उस वक्त करो उससे अगर तुमको भय लगे और भय नहीं लगे तो न मारो ! देवासुर संग्राम में राजा बलि और देवराज इन्द्र का युद्ध हुआ तो इन्द्र समझ गया कि राजा बलि मार डालेगा उठाया वज्ज्र और मार दिया। यह दृष्टांत कहने का मत- लब यह है कि तुम बैठे हो और चंचल होता है मन या विकार पंदा होते हैं तो इन विकल्पों से ग्लानि नहीं होती तो बज्ज्र न उठाओ और अगर ग्लानि होती है तो गाड़ दो वहीं पर । किस वक्त ? विचारों से कलनाओं के उदय, अनुदय से कल्पनाओं के भावाभाव में किस वक्त हर्ष-शोक न होगा ? जब 'में' के 'में' ही रहोगे तब। और जब तक कल्पनाओं से हर्न, शोक होता है भावा-भाव से तो समझना अभी स्थिति कच्ची है। अभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए एसा समझना । यह हथियार तो अस्वस्थता के लिए है। याने समझ तो लिया हैं 'में' आत्मा हूँ। मगर इस बोध की परिपाक अवस्था अभी नहीं हुई है। तो कल्पनाओं के उदय-अनुदय में हर्ष-शोक स्वाभाविक है। जहाँ मारे डण्डा तो न काम विकार रहेगा न लोभ रहेगा। किसो किस्म के विकार नहीं रहते । फट से शांत हो जाता है तो फिर ।
" न रूप मस्येह तथोपलभ्यते ……………… छित्त्वा "
संसार की जो जड़ है इतनी गहराई में गई है कि भगवान आत्मा रूपी शस्त्र के द्वारा ही कट सकती है। दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि संसार यदि मुझ से भिन्न हो तो कोई उपचार हो जब 'मैं'' ही प्रपंच हूं। मुझ आत्मा से प्रपंच की सत्ता भिन्न नहीं है तो ''मैं'' ही इसका नाशक भी हूं। सर्प के नाश का रज्जू हो शस्त्र है। उसी तरह संसार प्रपंच के नाश का मैं ही शस्त्र हूं। जैसे ध्यान में बैठते हो, पूजन पाठ में बैठते हो, तो सुन तो रहे हो, समझ भी रहे हो । जब तक यह संमझ बुद्धि को है तब तक कल्पनाओं के उदय-अनुदय में हर्ष शोक होगा ही । अरे.! बुद्धि भी तो एक कल्पना है। वृद्धि द्वारा मैंने समझा है कि में आत्मा हूं। मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं । (यह बुद्धि की धारणा है) तो भैय्या बुद्धि की समझ है तो फिर कल्पनाओं के उदय-अनुदय में हर्ष-शोक होगा ही और जब में उसको स्वयं समझेंगा तो स्वयं के समझने में कल्पना का सवाल ही नहीं । दूसरी चीज यह है. अगर अपने ही प्रतिबिम्ब से अपने को भय लगता है तो शीशा फेंक दो। अपने ही प्रतिबिम्ब से अपना मुख देखने पर शीशे में अपने आपको अपने ही प्रतिबिम्ब से भय लगता है तो फिर फेंक दो शीशा ।
'मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरम् ।
मनसो ह्यमनोभावे द्वंत नैवोपलम्यते ।' ।३१।
(गौ. पा. कारि. अद्वैत प्रकरण मंत्र सं. ।३१।)
जो कुछ चराचर प्रपंच है, सब मन है। तो मन हुआ शीशा मन अमनीभाव को प्राप्त हो गया तो जगत प्रपंच का भान ही कहां? तो मन है शीशा । जागृत अवस्था में और स्वप्नवस्था में जो कुछ दिखाई देता है प्रपंच, वह मुझ आत्मा का ही तो प्रतिविम्ब है। जाग्रत अवस्था में मन रहता है तो प्रपंच दिखाई देता है। स्वप्न अवस्था में मन रहता है तो प्रपंच दिखाई देता है। गाढ़ी निद्रा में मन नहीं रहता तो मन के न रहने पर अरे शीशा ही नहीं तो प्रतिबिम्ब कहाँ । अब यह पूछो कि यह शीशा कहां फेंके। अरे प्रपंच का मूल कारण जब मन हो है तो मन रूपी शीशा को कहाँ फेंके । सभी वेदान्तियों का कहना है कि मन सुषुप्ति में अपने कारण अज्ञान में लीन होता है और बड़े-बड़े वेदान्ती लोग ऐसा कहते हुए शिकायत करते हैं कि स्वामी जी ! विषय को समझ गया हूं मगर मन बड़ा परेशान करता है। तो फिर तुम समझ क्या गए हो ? तो यह बुद्धि द्वारा तुमने समझा है । अपने आप द्वारा नहीं समझा । में आत्मा के अज्ञान से मन है माने शीशा है । न कि स्वरूप ज्ञान में जब स्व-स्वरूप को जान लिया तो मन नाम की चीज ही नहीं है और दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण विभूति योग में कहते हैं-
'इन्द्रियाणां मनश्चास्मि'
जिसको मन कहते हैं वह मन 'में' हूं और मन का पाठ नपुंसक लिंग में पढ़ा जाता है और ब्रम्ह भी नपुंसक लिग है। तो हिजड़े- हिजड़े की लड़ाई है ।
ब्रह्म – ब्रह्माणि - ब्रह्मांसि और मनः मनसी - मनांसि ।
तो ये दोनों सजातीय हैं। मन की एकता प्रपंच से कभी नहीं हो सकती। मन की जब एकता होगी तो मुझ आत्मा से होगी। न स्त्री से, न शरीर से और न किसी पदार्थ से । मन का जो एकीकरण होगा तो मुझ आत्मा से ही होगा । पुत्र की एकता पिता से ही होती है न कि कुटुम्ब से । चाहे सैकड़ों आदमी हों घर में क्योंकि पिता ही है जो पुत्र नाम से कहा जाता है तो मैं ही हूं जो मन कहा जाता हूं। फेंक दो शीशा । मन का लय होना मन का अभाव नहीं है क्योंकि लय तो सुषुप्ति में भी हो जाता है। यह मन का अमन होना नहीं है। यानी लय होने से मन अमन हो जाय तो जाग्रत अवस्था में लौटकर न आवे । स्वरूपस्थ हो जाना मन का अमन होना है। मन के अमन हो जाने पर द्वैत प्रपंच की प्रतीति नहीं होती । मन का अपन हो जाना याने 'मैं' हो जाना ।
इन्द्रियों में जो मन है वह 'मैं' हूं। विचार, कल्पना, भावना, संकल्प, विकल्प इच्छा कामादिक विकार मन के ही नाना नाम हैं। पर्यायवाची नाम है। कभी मन विचार के रूप में दिखाई देता है कभी विकार के रूप में दिखाई देता है तो क्यों न भगवान का यह मंत्र पढ़ा जाय-
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि'
(भगवद्गीता अ.१० श्लो. ।२२। ')
'सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जयनामहं मनः ।
(श्रीमद्भागवत् एकादशस्कंध अध्याय १६ श्लोक ।११।)
'हौं हारयो करिजतन.... ... प्रेरक प्रभु बरजै ।।
(विनय पत्रिका)
मन का प्रभु, मन का राजा, मन का अधिष्ठान 'में' आत्मा ही तो हूं। मन का स्वामी होने के ही नाते, मन मुझ आत्मा के ही वश में रहता है। कहो-कैसे ? अरे ! मन मुझ आत्मा के वश में न हो तो दो घंटे सुबह और दो घंटे शाम दो से चार-सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का निरूपण होता है। तो अगर तुम्हारा मन तुम्हारे कहने सुनने में न चले । तुम्हारे वश में न रहे। तो इसको ग्रहण कैसे करोगे तुम । क्योंकि मन ही तो एक जरिया है। तो तुम भगवान आत्मा के वश में मन न होय तो विषय हृदयंगम् हो सकता है ? फिर भी शिका- यत करते हो- मन वश में नहीं है। कौन सा योग साधन मन को काबू में करने के लिए तुमने किया है ? यह 'मैं' की महिमा है। तो अभी जो यह निरूपण सुन रहे हो तो व्यवहार होकर सुन रहे हो कि अव्यवहार होकर । इसीलिए तुमको न मन का भान है न सुन रहे हो इसका भान है। मन के न रहने पर मन का व्यवहार भी • नहीं है। इसलिए में अव्यवहार्य हूं। बस इसी का नाम परमार्थ है।
'न निरोधो न चोत्पत्ति……………………….।
स्वामीजी ! एक प्रश्न है ? क्या है भैया ! मगर इस वक्त मुझे यह भान नहीं हो रहा है कि मैं मन का प्रेरक हूं- क्योकि में आत्मा हू । ठीक है। क्योकि में आत्मा हू । अरे ! भान न होना ही तो 'मैं 'हूं'। मैं आत्मा हूं। इसका भान न होना हो तो में हूं और यही मन के लिये प्रेरणा है। खूब समझो । खूब ग्रहण करो। यह तो जब याद दिलाई जाती है तब तुम जानते हो कि मैं सुन रहा हू। मगर सुन रहा हू, देख रहा हूं, जान रहा हूं, क्या इन क्रियाओ के क्रियाकाल में भी अनुभव होता है कि सुन रहा हूं, देख रहा हू, जान रहा हूं क्योंकि मैं आत्मा अव्यवहार्य हू और अव्यवहार्य देश में व्यव- हार को अनुभूति नही होती । देखना, सुनना यह सब व्यवहार है मगर व्यवहार के अनुभव काल में व्यवहार की अनुभूति का सर्वथा अभाव है क्योंकि में आत्मा अव्यवहार्य हूँ। इस अनुभूति को ही तो लेकर कारिका कहती है ।
न विरोधो न…………………………..।
यही परमार्थ है जो जिस काम में लगा है, वह इतना मस्त है। कि उस काम में, उसको भान ही नहीं होता कि मैं क्या हू और कुछ होय तब तो भान होय । सहज पद से देखोगे तब यह समझ में आएगा । उस वक्त कहा था न हमने दृष्टांत । साहब ! जो कुछ हम हैं वह सब जानते ही हो । वस्तुतः में क्या हूं. यह पता नहीं और इसी अवस्था में पशु, पक्षी, कीट पतंग नर-नारी, बाल युवा वृद्ध आस्तिक-नास्तिक, पापी-पुण्यात्मा, सन्त-असन्त सब इस स्थिति में बिना प्रयास के स्थित है। और सबके सब चींटी से लेकर ब्रम्हा पर्यन्त स्व-स्वरूप में स्थिर हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि तुम क्यों दिमाग्र खराब कर रहे हो। जब सब स्थित है तो तुम क्या समझा रहे हो । यही समझा रहे हैं कि बिना प्रयास के सब के सब स्वरूप में स्थित है और समझना इतना ही है। यह समझ भी पास में न रखना नहीं तो तुमको बेसमन दिखाई देगा । दूसरा ऐसी समझ में फिर न समझ है न बेसमझ है न बोध है न अबोध है न किसी किस्म का व्यवहार है। मगर समझ लेने के बाद व्यवहार नहीं है कि व्यवहार है ? कि व्यवहार है ही नहीं ।
इसलिए व्यवहार नहीं है । अरे भाई, व्यव- हार देश से व्यवहार है अव्यवहार देश से है ही नहीं। तो में भगवान आत्मा अव्यवहार्य हूं । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अनुभवकाल है। किसी व्यवहार के व्यावहारिक काल में कर्ता, कर्म क्रिया तीनों का सर्वथा अभाव है। क्यों अभाव है ? यदि मैं आत्मा व्यवहार होऊं तो व्यवहार का अनुभव हो। तो में आत्मा अव्यवहार्य होने के कारण किसी व्यवहार के व्यावहारिक काल में व्यवहार की अनुभूति नहीं होती ।
''नान्तः प्रज्ञं …………..... सविज्ञेयः ।''
अब चार बज रहे हैं, आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है।
ॐ पूर्ण मदः पूर्ण मिदं, पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते ।।
पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण मेवाव शिष्यते ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!
चतुर्थ दिवस का प्रवचन
(गुरुवार दिनांक १५ नवम्बर सन् १९७३ समय - १० बजे से १२ बजे ।)
अब पहले सारे उपनिषद के पाठ सुन लो फिर व्याख्या करें-
ओमित्येतदक्षरमिदंꣲ᳭ सर्व ।
आत्म जिज्ञासुओ, स्व-स्वरूप भगवान आत्मा के विशेषणों का विवेचन हो रहा है।
नान्तः प्रज्ञं ……………………….।
कल तक अव्यवहार्य की व्याख्या हुई थी । अब आज 'अलक्षणम्' में जो भगवान आत्मा हूं। अलक्षण कहते हैं, जिसका कोई लक्षण न हो । क्या कहा जाय ? जिसका कोई लक्षण न हो न 'मैं' आत्मा सत् हूं न असत हूं न जड़ हूं न चेतन हूं, न आनन्द रूप हूं, न दुःख रूप हू, न व्यापक हूं न परिच्छिन्न हू, न पूर्ण हूं न अपूर्ण हूं। मुझ आत्मा का कोई लक्षण है ही नहीं क्योंकि में अलक्षण हूं। 'मैं' आत्मा जैसा हू वैसा ही हूं। यदि कोई कहे ''मैं'' ऐसा हूं, यह भी एक लक्षण है। मैं अनिर्वचनीय हूं अवांडमनसगोचर हूं। वाणी मुझ आत्मा का कथन नहीं कर सकती । यदि में ऐसा कहें तो यह भी तो एक लक्षण है। ''मैं'' मन वाणी का विषय नहीं हूं यह भी एक लक्षण है। क्या यह कहा जा सकता है कि 'मैं' क्या हूं ? और कैसा हूं ? इसलिए किसी चीज का विरोध न करना ही मुझ आत्मा बा लक्षण है। यदि विरोध करते हो कि 'मैं' यह हूं और यह नहीं हूँ। यह लक्षण है तो विरोध ही करो । जो मर्जी आए कहो क्योंकि 'में अलक्षण हूं और यह अलक्षण विशेषण जो है इसकी अनुवृत्ति कहा से आती है "ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व" 'मैं'' सर्वं हूं, मुझ आत्मा से भित्र कुछ है ही नहीं तो भैय्या जब में सर्वः हूं तो जिसका जो लक्षण है. वह लक्षण मेरा ही तो है। ऐसा तो है ही नहीं कियह लक्षण मुझ आत्मा का है। ऐसा तो कहा जा सकता नहीं। तो अलक्षण की यही प्रभुता है, अलक्षण की यही अनुभूति है कि जैसा 'में' हू वेमा ही है।
"नासन्न सन्नः सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री, पुमान व नपुंसक मेक बोजम् ।।
यैर्बम्ह तत्समनु- पासितमेक चित्ताधन्या विरेजुरितरे भवपाश बद्धाः ।६।
न में सत् हूँ, न 'में' असत् हूं न में सत्-असत् हूं। न महान हूं न अणु सूक्ष्म हूं। न में स्त्री हूं न पुरुष हूं, न नपुंसक हूं। 'नासन सन्म ... .... भव पाश बद्धाः'
ऐसा जो सनातन ब्रम्ह आत्मा है, इसकी जो आराधना करते हैं वही धन्य हैं और ब्रम्ह उपासना (आत्मोपासना) से जो रहित हैं वे भवपाश में बंधे हुए हैं। इस गरज़ से मुझ आत्मा का कोई लक्षण नहीं है। अब प्रश्न होता है कि जब में आत्मा अलक्षण हूं, लक्षण- हीन हूं, कोई लक्षण नहीं है तो मुझ अधिष्ठान अलक्षण आत्मा में अध्यस्त जो प्रपंच है क्या इसका कीई लक्षण है ? 'में' अधिष्ठान आत्मा तो अलक्षण हूं। ठीक है, परन्तु मुझे अलक्षण आत्मा में प्रतिभासित माने अध्यस्त जो जगते प्रपंच है तो फिर यह भी तो अलक्षण ही है यदि कहो कि देह लक्षण वाला है, देह सत्य है ती देह को एक सा रहना चाहिए यदि कहो असत्य है तो दिखता क्यों है ? असत्य तो अभाव रूप होता है तो फिर कहो सत्य-असत्य दोनों है। तो यह भी कहते नहीं बनता। देहादिक प्रपंच न सत् है न असत् हैन सत्यासत्य है। अलक्षण है। कोई लक्षण ही नहीं। सब अलक्षण है। अब यह जो अलक्षणत्व धर्म है। तो यह अलक्षणत्व धर्म देह प्रपंच का है या मुझ आत्मा का है, आत्मा का है। डण्डे में जो लम्बापना, कालापना या खुर्दरापन है यह तो लकड़ी का ही है न भैय्या ! और यह भी सुन चुके हो जो अध्यस्त होता है वह अधिष्ठान के अनुरुप ही होता है। अधिष्ठान से अध्यस्त का भिन्न लक्षण नहीं होता । सोने में जो आभूषण है तो सोना अधिष्ठान है और आभूषण अध्यस्त है। तो सोने में पीलापना, वजनपना अधि- ष्ठान सोने का ही तो है । आभूषण तो फर्जी नाम है। तो पीला, वजन और मुलायमपना इसका नाम आभूषण है कि जो आकार- प्रकार है उसको आभूषण कहते हैं। मगर आकार-प्रकार में भी तो सोना है। सोने को अलग कर लेने पर आकार-प्रकार ही कहां रहेगा ? इसलिए जो लक्षण सोने का वही लक्षण आभूषण का । तो जो लक्षण मुझ आत्मा का वही लक्षण प्रपंच का । यदि 'में लक्षण वाला हूं तो देहादिक प्रपंच भी लक्षणवान हो यदि में आत्मा अलक्षण हूं तो प्रपंच भी अलक्षण है। इसका भी कोई लक्षण नहीं है । यह भी अवांग मनसगोचर है । इसका भी कोई लक्षण नहीं है। देखो, मन को । मन का क्या लक्षण है ? जिस तरह 'मैं' आत्मा निर्वयव हूं उसी प्रकार मन का भी तो आकार-प्रकार नहीं है कुछ। बुद्धि का आकार-प्रकार नहीं, चित्त का आकार-प्रकार नहीं। यदि आकार-प्रकार इस प्रपंच में दिखता भी है तो बिना मुझ अधिष्ठान आत्मा के आकार-प्रकार बनेगा किसमें ? और आकार-प्रकार का विकल्प होगा किस पर ? तो गर्ज यह है कि जिस तरह में 'आत्मा अलक्षण हूं तो उसी तरह देहादिक सारा प्रपंच भी अलक्षण है इसका भी कोई लक्षण नहीं है क्योंकि 'मैं' ही हूं। अच्छा। जो सारा प्रपंच जैसे कि में आत्मा अलक्षण हूं, उसी प्रकार देहादिक प्रपंच भी अलक्षण है तो यहाँ पर क्या कहोगे ? 'मैं' 'ही' हूँ कि 'मैं' हूँ ? तो 'ही' तो वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर कुछ भिन्न की प्रतीति होती है तो भिन्नता का अभाव करने के लिए ही 'ही' लगाया जाता है ।
अरे ! लकड़ी ही डण्डा है क्योंकि जब डण्डा कहते हो न, मालूम पड़ता है डण्डा और लकड़ी में भेद है। लकड़ी ही डण्डा है और लकड़ी में जब डण्डा खोजा तो डण्डा न मिला तो 'हो' निकल गया । डण्डा खोजने के पहले तो 'ही' लगेगा और लकड़ी देश में जब डण्डा ढूंढ़ा गया तो डण्डा न मिला तो जब डण्डा है ही नहीं तो लकड़ी है। तो 'ही' किसके लिए लगाओगे, तो 'ही' कहाँ रहेगा फिर तो 'ही' निकल गया। तो अब रहेगा- लकड़ी है। यह बाध है। तो दरिद्र प्रपंच का निःसारण करने के लिए भगाने के लिए 'ही' लगाया जाता है। सोना ही आभूषण है धागा ही वस्त्र है, लोहा ही शस्त्र है। और जब सोने में आभूषण न मिला तो सोना है। 'ही' निकल गया । इसी तरह प्रपंच को देखकर प्रपंचाभाव करने के लिए जब प्रपंच की प्रतीति होती है तो प्रपंच का अभाव करने के लिए 'अहमेवेदम्सर्वम्' आत्मैवेदम्सर्वम्, ब्रह्मवेदम् सर्वम्, वासुदेवेदम् सर्वम् सब आत्मा ही है, सब नारायण ही है, सब में ही हूँ। जब दरिद्र निकल गया। तो 'मैं' हूँ। 'ही' की जरूरत नहीं रही। इसी तरह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं, स्थूल- सूक्ष्म कारण तीनों शरीर सत्, रज तम तीन गुण । बस दरिद्र भाग गया। जब दरिद्र निकल गया तो मैं हूँ। अब लक्षण कौन बताएगा बरे ! प्रपंच देश से लक्षण का विकल्प होता है या निष्प्रपंच देश से? प्रपंच देश से लक्षण का विकल्प होता है। दरिद्र देश से । संसार प्रपंच के ही अंदर धनवान और दरिद्र होते हैं और भंगवाने देश में तो न कोई दरिद्र है न धनवान है। बिना "अलक्षण" स्वरूप के बोध के बिना यह दरिद्र जाता ही नहीं । जिसका एक बालक नहीं वह भी दरिद्र और जिसके ज्यादा है वह भी दरिद्र । अब समझलो । सब अनुभवशील बैठे हो । जिसका रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बह भी दरिद्र और जिनके बड़े-बड़े विल्डिग बने हुए हैं वे भी दरिद्र हैं। जिसके यहाँ खाने को नहीं वह भी दरिद्र बौर जिसके पास लाखों हैं वह महा दरिद्र । अब दरिद्र कौन नहीं है--
"ब्रह्मानंद रसं पीत्वा येतु उन्मत्त योगिनः ।
इन्द्रोऽपि रंकवत् भाति का कथा नृप कीटकाः " ॥
ब्रह्मानंद मदिरा को पीकर जो उन्मत्त है उनकी दृष्टि में इन्द्र भी भिखारी के समान दिखाई देता है। वही भर दरिद्र नहीं है। और तो सारा संसार दरिद्र है। तो जब तक प्रपंच के प्रति आस्था है। जब तक प्रपंच का अस्तित्व है। तो भैया वह दरिद्र ही है।
"नारायणे वेदम् सर्वम्, अहमे वेदम् सर्वम् ।"
वासुदेवः सर्व मिति । वासुदेव ही सर्व है और जब दरिद्र निकल गया, जब अपने आत्मदेश में ढूंढ़ा तो प्रपंच न मिला तो 'हा' निकल गया । तो 'में' हूँ रह गया। यहाँ पर 'में' आत्मा 'अलक्षण' सिद्ध होता हूँ। "ही" निकल जाने पर इस स्थान में 'मैं' आत्मा बलक्षण सिद्ध होता हूँ प्रपंच के रहते नहीं । प्रपंच में रहते पर तो नाना लक्षण वाला में आत्मा प्रतीत होता हूँ। वाह ! जो अपने को साढ़े तीन हाथ का मानता हैं उसको साढ़े तीन हाथ का ही लक्षण वाला दिखता है। तो फिर इतने लक्षण है कि अनन्त । जो अपने आपको संसारी जीव मानता है उसको जीव सा दिखता हूँ। देह मानने वाले को देह सा दिखता हूँ। स्त्री मानने वाले को स्त्री सा दिखता हूँ। पुरुष मानने वाले को पुरुष सा दिखता हूँ। आस्तिक को आस्तिक सा और 'है' को 'है' सा और नहीं को 'नहीं' सा । ये जितने लक्षण हैं; ये प्रपंच देश के विकल्प हैं। जो प्रपंच म रहता है उसकी जैसी धारणा होती है उसके लिए 'मैं' आत्मा वैसे ही प्रतीत होता हूँ । वस्तुतः वैसा 'मैं' नहीं हूँ। यदि आत्मा होकर या 'में' होकर 'मैं' को देखा तो 'मैं' आत्मा में किसी किस्म का लक्षण नहीं है। परन्तु अपने आप को कुछ मानकर वह देखता है इसलिए कोई न कोई लक्षण देखता है तब वह लक्षण बताता है। श्रुतियाँ भी तो सनातन ब्रह्म आत्मा के लक्षण का विवेचन करती है।
"न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ।
ज्ञान प्रसादेन विशुद्धसत्त्वत्प्त्त तस्तु तं पश्यते निष्कलंध्यायमानः " ॥८॥
(मुण्डक उप० (तृतीय) खंड प्रथम मं० सं० ॥८॥)
"एष देवो विश्व कर्मा महात्मा सदा जानानां हृदये संनिविष्टः ।
हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति ।१७।
(श्वेताश्वतरोपनिषद् अध्या० ४ मं० सं० ॥१७॥)
ये सब लक्षण ही तो हैं। परन्तु श्रुतियाँ जो हैं इन बेचारियों को क्या कहा जाय ? क्योंकि श्रुतियाँ, वाणी रूप हैं और वाणी का वहाँ गम नहीं है। तो श्रुतियाँ जो लक्षण बताती हैं वह भगवान आत्मा को 'इद् मित्थम्' ऐसाही है कहने में कोई श्रुति समर्थ नहीं है।
रामायण में चापाई आती है कि--
आदि अंत कोऊ जासु न पावा, मति अनुमान निगम असगावा ।
अपनी बुद्धि के अनुसार । परन्तु जैसा है वैसा ही है। इस चौपाई में अलक्षण भी है और लक्षण भी "आदि अंत कोऊ जासु न पावा" यह जैसा है और मति अनुमान निगम अस गावा “यह ऐसा है । इद मित्थम् कहि जाय न सोई" इसलिए 'मैं' आत्मा अलक्षण हूँ। कोई भी कहने में समर्थ नहीं है। और मुझ आत्मा के अति- रिक्त जो कुछ भी है, सब विकल्प ही तो है और विकल्प सत्ताहीन होता है। तो सत्तावान का लक्षण वह क्या बता सकता है ? श्रुतियां स्मृतियां सत्ताहीन हैं । इनका अस्तित्व ही नहीं है। मुझ सत्तावान आत्मा का लक्षण कोई क्या बता सकता है ? इसलिए अलक्षणम् । और मुझ अलक्षण आत्मा का लक्षण बताना अरे अल- क्षण पर कलंक है, लॉछन है। जी हाँ ! और बताने तक ही तो है वह । श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, शास्त्र वेद लक्षण बताने तक ही तो जिन्दा भी हैं और कहते-कहते जब पार न मिला स्वयं ही अलक्षण हो जाते हैं। क्या कोई कह सकता है ? देखो - देह है। देह 'है'। यह जो "है" है यही सत्ता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इसको "युनिव्हर्सल ठूथ" कहते हैं। व्यापक सत्य । यह अस्तित्व इतना ठोस है। इतना घन है। वाह । माने यह जो है 'है' अस्तित्व है, यही सत्ता है। 'हैं' हुआ अधिष्ठान और सारा प्रपंच हुआ अध्यस्त और यह हम पहले बता चुके हैं कि जो अध्यस्तु पदार्थ होता है, वह अधिष्ठान के अनु- रूप ही होता है, अधिष्ठान स्व-स्वरूप ही होता है। अधिष्ठान से अध्यस्त की सत्ता भिन्न नहीं होती । तो जिस तरह अधिष्ठान के लिए ऐसा नहीं आता उसी तरह अध्यस्त प्रपंच के लिए भी 'ऐसा' नहीं आएगा 'शिव' हां जी ! जिस प्रकार अधिष्ठान, उसको कहते हैं जिसके बिना जो न रहे, वही उसका अधिष्ठान है। लकड़ी के बिना डण्डा नहीं रह सकता इसलिए डण्डे का अधिष्ठान लकड़ी है। तो उसी तरह यह जो 'है' हे, अधिष्ठान । यह अधिष्ठान 'है' है और सारा चराचर देहादिक प्रपंच यह सब प्रपंच है। तो 'है' माने अधिष्ठान 'है' अधिष्ठान पर जैसे कि लकड़ी में डण्डा, उसी तरह अस्तित्व में देह है। जिसके बिना प्रपंच की सिद्धि न होय वही प्रपच का अधि- ष्ठान है। जैसे लकड़ी के बिना डण्डे की सिद्धी नहीं इसलिए डण्डे का अधिष्ठान लकड़ी है । तो 'है' के बिना कुछ है ही नहीं । प्रपंच है, देह है, मन है, बुद्धि है, चित्त है। एक तिनका से लेकर ब्रम्हा पर्यंत । सत्य है, असत्य है, जड़ है, चेतन है, व्यापक है, खंड है, पूर्ण है, अपूर्ण है जीव है, ब्रम्ह है। तो यह जो अस्तित्व है, सत्ता पद है, उस अस्तित्व पर जो कुछ मन वाणी का विषय है वह सब अध्यस्त है। और यह कल्पित प्रपंच है। अच्छा तो । माने। जैसे-लकड़ी के बिना डण्डा नहीं, सोने के बिना आभूषण नहीं, उसी तरह अस्तित्व के बिना प्रपंच नहीं । अच्छा-अब यह समझना है कि जैसे अस्तित्व अलक्षण है, 'जैसा है', उसी तरह से प्रपंच भी 'जैसा है' ऐसा नहीं है। अब प्रश्न होता है- अधिष्ठान 'है' के बिना अगर 'ऐसा' सिद्ध हो जाय अब ऐसा जो दरिद्र है इसका निस्सारण करना है। 'है' जो अस्तित्व है, 'सत्ता' उसके बिना 'ऐसा' सिद्ध हो जाय, तब तो ऐसा है। अरे ! ऐसा है कहते हो कि नहीं ? तो ऐसा को कौन सिद्ध करता है। 'है' सिद्ध करता है तो 'ऐसा' कहां है ? अरे, 'है' के बिना ऐसा भी तो नहीं । 'ऐसा' जो शब्द है उसको कौन सिद्ध करता है? 'है' तो फिर 'है' अधिष्ठान पर ऐसा भी तो अध्यस्त है। तो 'हैं' के बिना ऐसा को कौन सिद्ध करेगा। इसलिए ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। 'है' ही है। तो भैय्या - यह सब अस्तित्व ही भास रहा है प्रपंच नहीं भास रहा है। लकड़ी देख रहे हो, डण्डा नहीं देख रहे हो। तो 'मैं' अस्तित्व आत्मा ही हूं। अस्तित्व, 'आत्मा' । यहाँ पर बुद्धि खोजाती है। 'ऐसा' को बुद्धि ग्रहण करती है न । जब 'ऐसा' भी निकल गया तो अस्तित्व का अस्तित्व ही तो रह गया शेष । शान्त पद है यह। यहां पर 'अलक्षणत्व धर्म' सिद्ध होता है। अब कहोगे - साहब, देह तो आकार प्रकार वाला है तो फिर वही युक्ति आएगी । हाथ है, पांव है, कान है, नाम है । 'है' के बिना आकार और प्रकार तुम्हारा सिद्ध हो तो जाय । किसी की सिद्धि नहीं, अस्तित्व के निकाल लेने पर तो जो कुछ. है, 'है' ही है। अस्तित्व ही है। त्रपंच है, डण्डा है। तो डण्डा कहने से डण्डे का बोध होता है कि डण्डा कहने से लकड़ी का ? तो प्रपंच है, तो प्रपंच कहने से अरे, प्रपंच का बोध होता है। कि अस्तित्व का ज्ञान होता है तो जब अस्तित्व का ज्ञान होता है तो जिस तरीके से 'मैं' अस्तित्व आत्मा अलक्षण हूं। तो इस प्रपंच का भी कोई लक्षण नहीं है। अरे ! प्रपंच देश से लक्षण की सिद्धि होती है न । किसी के लक्षण की सिद्धि प्रपंच देश से होती है। डण्डा ऐसा होता है, सीधा होता है, चौड़ा होता है तो डण्डा देश से लक्षण कहा जाता है तो प्रपंच देश से भगवान आत्मा का लक्षण बताया जाता है परन्तु आत्म देश में देखो तो लक्षण है ही नहीं तो कहां से बत्ता- एगा । बताने वाले सब दरिद्र (मान्यताएं) तो भाग गए इसलिए 'अलक्षणम् 'मैं'' आत्मा अलक्षण हूं और फिर बात यह है न, कि यदि अगर मेरे मुंह, सींग, पूंछ होते तो भगवान में भी सींग, पूंछ की कल्पना होती । जो जैसा अपने आपको मानता है वही मान्यता भगवान पर भी आरोपित करता है। यह अटल सिद्धांत है। जो जैसा अपने आपको मानता है, तो वही मान्यता, अलक्षण भगवान आत्मा पर भी आरोपित करता है, कि भगवान ऐसा' है। अगर में हिन्दू मानता हूं अपने को तो भगवान को भी शिखा, सूत्र वाला मानता हूं कि भगवान भी चंदन लगाते हैं वह भी जनेऊ पहिनते हैं। अगर हमारा व्याह होता है तो उनका भी व्याह होता है मगर भगवान आत्मा जैसा है वैसा ही है। वह अछूता है यह तो हमारी धारणा है। हमारा विकल्प है, हमारी कल्पना है कि मैं भगवान को इस प्रकार से मानता हूं मगर वह जैसा है वैसा ही है ।
'ईसाई में गो ईसाई सा है, ईसाई वो तो मशहर ही नहीं
हिंदू में हिंदू सा दीख पड़े, वले हिंदू पने का असर ही नहीं
इस्लाम में वो इस्लाम सा है बांधे दीन की कोई कफ ही नहीं ।
हर जात में जात उसी की है, पर जात की उसको खबर ही नहीं।'
तो भगवान आत्मा की वास्तविकता का पता कैसे लगेगा ? भगवान होकर देखो । भगवान की हकीकत याने सच्चाई का पता कैसे लगेगा कि भगवान कैसा है ? भगवान होकर देखो ।
अगर किसी की सच्चाई का पता लगाना है तो उससे अलग होकर पता नहीं लगा सकते जबकि वही न हो जाओ । हां, जो बड़े बड़े शतियां बदमाश होते हैं, अच्छे-अच्छे काबिल, तो गव्हर्नमेन्ट की तरफ से जो सी. आई. डी. डिपार्टमेन्ट होता है तो चोर का पता लगाने के लिए उसकी फोटो रखता है. अपने साथ में और साथ में उसके चोरी करने जाता है, अपने हाथ में हथकड़ी भी पहन लेता है और चोर के साथ जल भी जाता है क्योकि विभाग ही ऐसा है । भैय्या ! चोर पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है वैसे बाहर से पता नहीं लगा सकता क्योंकि जो चोर होगा वह चोर ही बताता है कि मैं चोर हू, कातिल हूं इसी तरह भगवान लक्षण वाला है कि, अलक्षण है। भगवान कैसा है, इसका पता लगाने के लिए भगवान ही होना पड़ता है तो फिर भगवान होना क्या है ?
अरे ! कुछ न होना यही भगवान होना है, कुछ भी न बनना यही भगवान होना है अपने मे को कुछ मानकर भगवान कैसा है। इसका पता नहीं लग सकता। अपने 'मैं' को कुछ मानकर तुमने अपने आपको कुछ न माना 'मे' का मैं ही जाना तो 'में' को मैं' हो जानना यहां वास्तव में भगवान होना है और 'मैं' को कुछ मान लेना यही बनना है। इसको बनना कहते हैं तो दरअसल में. 'आत्मा' लक्षण- वान हूं कि अलक्षण हूं इसको पता लगाना है। अलक्षण का दर्शन करना है तो फिर जैसे हो वैसे हो रहो । बनो मत । देखो ! मुसलमानों के यहां शिष्टाचार के रूप में कोई बड़े आदमी के पास जाता है तो कहता है हुजूर में तो एक नाचीज हूं यह उनका शिष्टाचार है। यह खाकसार नाचीज है।
कितना सुन्दर मौके की चीज है मैं तो नाचीज़ हूँ। माने में कुछ नहीं हूँ, । अगर में कुछ कहूँ कि में फलाँ हूँ, याने अमुक हूँ इस लिए में कोई चीज नहीं हूँ। जो हूँ, सोई हूँ कितना सुंदर भाव भरा हुआ है इस शब्द में । हुजूर में तो नाचीज हूँ तो भैय्या नाचीज तो भगवान के सिवाय दूसरा नहीं । अरे ! भगवान भी तो नाचीज है कहो कि ऐसा है तो ऐसा नहीं है तो लक्षण तो चीज़ में होती है, नाचीज जो होता है अलक्षण होता है-जैसे अपने आपको माना कि मैं देह हूँ तो देह का लक्षण तुमको बताना पड़ेगा यदि जीव कहोगे तो जीव का भी लक्षण है। जोव अल्पज्ञ है, जीव पुण्यात्मा है, पापी है, जीव छोटा होता है और अनेक होता है। परिच्छिन्न होता है। ये सब जीव के लक्षण हैं। अपने 'मैं' को जीव मानों तो जीव का भी लक्षण है और ब्रम्ह मानो तो इसका भी लक्षण है-व्यापक है, अखंड है, सत् है, चित है, आनन्द है ये सब ब्रम्ह के लक्षण हैं। यह भी एक चीज है और चीज न हो तो लक्षण न हो । अरे, भाई ब्रम्ह का लक्षण बहते हैं न, व्यापक है, पूर्ण है, सत् है, चित् है आनन्द है, तो 'ब्रम्ह' हुआ एक 'चीज' और 'चीज' होने से ब्रम्ह का भी लक्षण है। जैसे कोई कहता है मैं 'पुरुष हूँ तो पुरुष का भी लक्षण है। कोर्ड कहता है में स्त्री हूँ तो स्त्री का भी लक्षण है, गरज यह है कि अपने को कोई चीज मानोगे तो उस चीज़ का कोई न कोई लक्षण जरुर होगा और जिस वक्त मै 'नाचीज़' हूँ तो नाचीज 'अलक्षण' का परियायवाची शब्द है। मैं का मैं ही रह गया । इसलिए श्रुति कहती है अलक्षणम् । कोई लक्षण नहीं है। जब 'मैं' आत्मा अलक्षण हूँ, तो मुझ आत्मा पर यह जो चराचर प्रपंच है यह भी अलक्षण है, इसका भी कोई लक्षण नहीं है। प्रपंच नहीं है इसलिए प्रपंच अलक्षण है और 'में, हूँ' इसलिए अलक्षण हूँ । प्रपंच नहीं है जब हो तब न लक्षण है। जब प्रपंच है ही नहीं तो लक्षण क्या होगा । इसलिए प्रपंच अलक्षण है । तब मुझ आत्मा का लक्षण कौन बतावे ? अरे ! जो लक्षण बताने वाला था वह तो चला गया । अब मुझ आत्मा का लक्षण कौन कहे ।
लक्षण से अलक्षण है कि अलक्षण से लक्षण है ? लक्षण से अलक्षण है माने लक्षण-अलक्षण को सिद्ध करता है कि अलक्षण- लक्षण को सिद्ध करता है ? फिर एक बार सुनो-प्रपंच भाव रूप है। कि अभाव रूप ? अभाव रूप । तो अभाव रूप होने के नाते प्रपंच लक्षणवान है कि अलक्षण है। क्योकि जब है ही नहीं तो उसका लक्षण क्या होगा ? इसलिए प्रपंच अलक्षण है और जब प्रपंच है ही नही तो मुझ आत्मा का लक्षण कौन बताएगा कि भगवान आत्मा ऐसा है । देहादिक प्रपंच-ससार प्रपच, जगत प्रपंच ये अभावरूप हैं। कि भावरूप ? अभाव रूप । अभावरूप होने के कारण प्रपंच अलक्षण है क्योकि जब होय तब न, उसका लक्षण बने । तो जब है ही नहीं तो प्रपंच लक्षण क्या होगा इसलिए प्रपच-अल- क्षण है और 'मै' इसलिए अलक्षण हूँ कि बताने वाला कोई नहीं अलक्षणम् । में भगवान आत्मा अलक्षण हूँ। ये सब विलक्षण चीजें हैं भैया !
"नान्तः प्रज्ञं……………………………..।
प्रपंच में जो अलक्षणत्व धर्म है, यह मुझ अधिष्ठान का है कि प्रपंच का ? अधिष्ठान का । क्योंकि प्रपंच को अलक्षणत्व धर्म दिया किसने ? मैंने दिया । याने अभाव रूप है न । बन्ध्या पुत्र वत् शशश्रृंगवत् प्रपंच को जो कहा गया है कि प्रपंच अलक्षण है ताे अलक्षण है तो अलक्षण भी तो नहीं कह सकते क्योंकि जो है ही नहीं उसको अलक्षण कैसे कहा जा सकता है। अभाव रूप प्रपंच को अलक्षणत्व धर्म मिला कहाँ से ? मुझ आत्मा से। क्योंकि मुझ आत्मा अधिष्ठान पर ही तो प्रपंच अध्यस्त है अलक्षणत्व धर्म तो मुझ आत्मा का ही है।
गुरुवार दिनांक १५ नवम्बर सन् १९७३ समय २ बजे से ४ बजे ।
नान्तः प्रज्ञं ……………………………. सविज्ञेयः ।
उस समय अलक्षण का विवेचन हुआ था। अब इस समय अचिन्त्य का है 'मैं' भगवान आत्मा अचिन्त्य हूँ । भैया ! अचिन्त्य कहते हैं। जिसका चिन्तन न किया जा सके । अब प्रश्न होता है आत्म चितन किसे कहते हैं ? जिसका चिंतन न होय उसको अचि- स्व कहते हैं। तो आत्म चिंतन, भगवत् चिन्तन क्यों कहा जाता है और श्रुति कह रही है- अचित्य है। चीज़ यह है कि एक चिंतन तो हाता है चित्त से। तो यदि चित्ता करके आत्मा का चिन्तन माना जय तो फिर वह अचिन्त्य नहीं क्योंकि चित्त से जो चिन्तन होता है वह चित्त का ही होता है। बिना चित्त से जो चिन्तन होता है वह 'चित' का चिन्तन है। चित्त का जो चिन्तन होता है वह विक- ल्प का चिन्तन होता है। जो वैकल्पिक पदार्थ होता है, जिसके आकार-प्रकार का विकल्प किया जाता है। चाहे जो भी वीज हो। स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो । जो वैकल्पिक पदार्थ होता है उसका चिन्तन चित्त से होता है। और उसका सम्बन्ध चित्त के निरोध से होता है। जब तक वित्त का निरोध है तो चित्त के निरोध-काल तक ही उसका चितन है और चित्त जब चंचल हुआ तो वह चिन्तन भी गया। वह चिन्तन नहीं रहता 'एक' दूसरी चीज़ यह है कि यावत्काल चित्त है। चित्त जागृत अवस्था म भी रहता है और स्वप्न में भी रहता है। जब तक वह चित्त है तब तक बह चित्त- गम्य है और चित्त का ही बनाया हुआ वह चिन्त्य है। वह चित्य चित्त करके ही कल्पना किया हुआ है। चित्त का हा वह दूसग स्वरूप है। चित्त द्वारा जो कल्पना किया हुआ चिन्त्य पदार्थ है ।
तो आचिन्त्य कहते हैं आत्मा को और चिन्त्य नाम प्रपंच का है। प्रपंच चिन्त्य है और आत्मा अचिन्त्य है। जी हाँ ! तो चित्त द्वारा जो काल्पनिक पदार्थ है, तो उसका चिन्तन चित्त के निरोध से संबंधित है। चित्त को रोक कर ही उस पदार्थ का चिन्तन किया जा सकता है अन्यथा नहीं । चाहे कोई देवी हो चाहे देवता हो, चाहे कोई नर हो चाहे नारी हो । गरज यह है कि चित्त द्वारा जिसका चिन्तन किया जाता है वह काल्पनिक है, नश्वर है और वह माना हुआ है। इसलिए बिना चित्त के उसका चिन्तन नहीं हो सकता। यहाँ पर अचिन्त्य का चिंतन करना है। 'मैं' आत्मा जो हूँ, अचिन्त्या हूँ । जब आत्मा अचिन्त्य है, तो अचिन्त्य के चिंतन, का क्या स्वरूप है ? जैसे कोई कल्पना करता है। जिसका जो इष्ट होता है उस इष्ट के नाम-रूप की कल्पना करके, जो जिसका इष्ट होता है जैसे-भगवान विष्णु हुए, शिव हुए, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए शक्ति हुई। ऐसा नाम है रूप है और उस काल्पनिक इष्ट की हृदय में धारणा करके चित्त में उसका चिन्तन करता है। उस आकार-प्रकार वाले इष्ट का चित्त ही आधार है। क्योंकि वह चित्त का ही माना हुआ है। तो जब तक चित्त एकाग्र न होगा तब तक हृदय में उस आकार-प्रकार वाले इष्ट का चिंतन हो नहीं सकत्ता और यही कारण है कि कोई जब ध्यान करने के लिए बैठता है, अपने इष्ट का और चित्त जब चंचल हो जाता है तो हृदय में जबर्दस्त ग्लानि होती है तब सोचता है कि किसी संत महात्मा के पास जाकर चित्त की स्थिरता का साधन पूछें जब उसका आधार ही न रहेगा तो वह इष्ट कहाँ रहेगा? भाई : हृदय में तो बड़ा दुःख होता है, ऐसे ध्यान में। क्योंकि अचिन्त्य का तो कभी विचार किया नहीं और चिन्त्य अचिन्त्य नहीं । यानी मतलब यह है कि अचिन्त्य का चिन्तन उससे होता नहीं । अचिन्तन का चिन्तन होता नहीं और चिन्त्य के चितन में चित्त एकाग्र नहीं होता इस तरह दोनों तरह मुसीबत है न । तात्पर्य यह है कि अचित्य का चिन्तन नहीं, अचिन्त्य चिन्तन उससे होता नहीं और चिन्त्य के चिन्तन में उसका चित्त एकाग्र नहीं, इसीलिए होती है, ग्लानि । अचिन्त्य का चितन उससे नहीं होता जिसकी काल्पनिक इष्ट में निष्ठा होती है, जिसकी उसमें श्रद्धा है वह अचिन्त्य से बहुत दूर है । नाम रूपात्मक, आकार प्रकार वाला जो चिन्त्य है उसका चितन बिना चित्त एकाग्र हुए होता नहीं तो साधक को इतनी ग्लानि होती है कि उसका साक्षी स्वरूप है ? जैसे कोई कल्पना करता है। जिसका जो इष्ट होता है उस इष्ट के नाम-रूप की कल्पना करके, जो जिसका इष्ट होता है जैसे-भगवान विष्णु हुए, शिव हुए, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए शक्ति हुई। ऐसा नाम है रूप है और उस काल्पनिक इष्ट की हृदय में धारणा करके चित्त में उसका चिन्तन करता है। उस आकार-प्रकार वाले इष्ट का चित्त ही आधार है। क्योंकि वह चित्त का ही माना हुआ है। तो जब तक चित्त एकाग्र न होगा तब तक हृदय में उस आकार-प्रकार वाले इष्ट का चिंतन हो नहीं सकत्ता और यही कारण है कि कोई जब ध्यान करने के लिए बैठता है, अपने इष्ट का और चित्त जब चंचल हो जाता है तो हृदय में जबर्दस्त ग्लानि होती है तब सोचता है कि किसी संत महात्मा के पास जाकर चित्त की स्थिरता का साधन पूछें जब उसका आधार ही न रहेगा तो वह इष्ट कहाँ रहेगा? भाई : हृदय में तो बड़ा दुःख होता है, ऐसे ध्यान में। क्योंकि अचिन्त्य का तो कभी विचार किया नहीं और चिन्त्य अचिन्त्य नहीं । यानी मतलब यह है कि अचिन्त्य का चिन्तन उससे होता नहीं । अचिन्तन का चिन्तन होता नहीं और चिन्त्य के चितन में चित्त एकाग्र नहीं होता इस तरह दोनों तरह मुसीबत है न । तात्पर्य यह है कि अचित्य का चिन्तन नहीं, अचिन्त्य चिन्तन उससे होता नहीं और चिन्त्य के चिन्तन में उसका चित्त एकाग्र नहीं, इसीलिए होती है, ग्लानि । अचिन्त्य का चितन उससे नहीं होता जिसकी काल्पनिक इष्ट में निष्ठा होती है, जिसकी उसमें श्रद्धा है वह अचिन्त्य से बहुत दूर है । नाम रूपात्मक, आकार प्रकार वाला जो चिन्त्य है उसका चितन बिना चित्त एकाग्र हुए होता नहीं तो साधक को इतनी ग्लानि होती है कि उसका साक्षी वह स्वयं है और प्रायः ज्यादा तादाद में चिन्त्य के ही चिन्तन करने वाले पाए जाते हैं। अचिन्त्य चिंतन करने वाले तो बिरले ही होते हैं। क्योकि अचिन्त्य का चितन बिना स्वरूपात्मा के बोध हुए नितांत असंभव है। अचितन का चितन तो वही कर सकता है जिसने अचिन्त्य दर्शन किया है और चिन्त्य का चिन्तन तो सुन करके ही होता है, देख करके नहीं होता । सुनते हैं कि भगवान राम का स्वरूप ऐसा है, शक्ति ऐसी है । तो सुना है, देखा तो नहीं है। न चित्र बनाने वाला ही उसको देखा है सिर्फ कल्पना है । तुम जो चित्र देखते हो किसी भी देवता का, वह चित्रकार की कल्पना ही तो है । तात्पर्य है कि, सुनकर के वैसे ही कल्पना कर ली जाती है और फिर चित्त द्वारा उसका चितन करते हैं परन्तु अचिन्त्य का तो चिंतन होता है दर्शन करके । अब यहाँ पर समझना है कि अचिन्त्य का चिंतन । अचिन्त्य-चितन का चित्त के निरोध और अनिरोध से कोई सबंध नहीं है क्योंकि अचिन्त्य-भगवान का चितन है, वह चित्त की एकाग्रता और उसके निरोध से स्वरूप भगवान आत्मा का कोई संबंध नहीं है । अब आत्म चिन्तन का स्वरूप बताएंग और उसमें बिठालेंगे ।
चित्त के निरोध में जो चिंतन होता है उसमें देशकाल की सीमा है। कहाँ पर चिंतन करें ? चिन्तन के लिए एकांत की जरूरत पड़ती है। एकान्त कमरा हो । कोई हल्ला-गुल्ला न हो सुन-सान हो। किस वक्त करना चाहिए तो चित्त का निरोध करके जो चितन किया जाता है उसके लिए देशकाल की सीमा नहीं रहती, भगवान आत्मा का चितन हर वक्त होता है, क्योंकि अचिन्त्य के चित्तन के लिए चित्त एकाग्र हो तब क्या, चित्तचंचल हो तब क्या ? चित्त की एकाग्रता चंचलता से उसका संबंध नहीं है। श्रीकृष्ण भगवान तो यहां तक अर्जुन से कहते हैं-
"तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च ।
मर्यापत मनो बुद्धिर्मा मेवैष्य स्यसंशयम् ॥
।। गीता अ. (८) ।। 11
भगवान ने कितनी आजादी दे रखी है अर्जुन को । अर्जुनः सर्वकाल में मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर । युद्ध ऐसा कठिन कार्य है, जबकि युद्ध करने वाले पर इतनी जिम्मेदारी होती है, अपनी रक्षा, रथ की रक्षा सारथी की रक्षा, घोड़ों की रक्षा और शत्रु को मारना । यह सब कार्य करते हुए भगवान का चिंतन । भगवान ने यह तो नहीं कहा कि दिन भर तो युद्ध हो रहा है । और जब युद्ध बंद हो तब एक दो घंटे शाम को मेरा स्मरण कर । (आज कल युद्ध का कोई समय नहीं है परन्तु पुराने जमाने में शाम होने पर दोनों तरफ से शंख बज जाते थे और लड़ाई बंद हो जाती थी । सब सैनिक अपने-अपने वैरकों में चले जाते थे। खाना पीना, आराम करना और सबेरे युद्ध में डट जाते थे) ऐसा नहीं अहा। "सर्वेषु, कालेषु" अर्थात् सर्वकाल में- जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति में, मूर्च्छा और समाधि में, तथा सुख-दुःख में । मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। कैसा चिंतन है भाई ! तो भैया : वह कौन सा स्मरण है ? 'माम्'-कोडर्थ : ? आत्मानम् ! माम्-यह कर्म कारक है। सर्वकाल में मुझ आत्मा का स्मरण भी कर और थुद्ध भी कर । क्योंकि आत्मा ही-
'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित :
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च।२०।
(गीता-अ. १० श्लोक २०)
अर्जुन सारे चराचर में स्थित जो आत्मा है, वह मैं हूँ। जिसका विवेचन हो रहा है, चार दिन से । 'माम्' शब्द कर्मकारक है, सर्व- काल में मुझ आत्मा का स्मरण भी कर और युद्ध भी कर । तो भैय्या' सर्वकाल में उसी का चितन हो सकता है जो सर्वकाल में होगा । और कभी रहे और कभी न रहे, तो सर्वकाल में उसका चितन नहीं होता और काम-काज करते हुए भी नहीं होता क्योकि ऊधोः मन न भए, दस बीस ! और एक ही काम करेगा एक वक्त में चाहे युद्ध ही कर चाहे स्मरण कर अगर सर्वकाल में भगवान का चितन होता है, उस चिन्तन का संबंध चित्त से होता तो सर्वकाल में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, ऐसा नहीं कहते । इससे प्रत्यक्ष है कि भगवत चिन्तन का सम्बन्ध मन से नहीं है। इसलिए जो पदार्थ सर्व- काल में रहता है उसका सर्वकाल में चितन हो सकता है । जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा और समाधि आदि अवस्थाओं में । अच्छा। फिर देखो-यदि समाधि अवस्था को आत्म चिन्तन की अवस्था मानी जाय और समाधि ही आत्म चिन्तन होता तो फिर असमाधि में आत्म चिंतन नही होता ऐसा माना जाय तो सर्वकालीन स्मरणन हुआ और दूसरी बात तो भगवान ने इसमें कहा है-समाधि में युद्ध ।। समाधि में तो न युद्ध होय न देखना होय, न सुनना होय जिसको कि लोग समाधि कहते है क्योंकि मन के निरोध हो जाने पर इन्द्रियाँ भी निरुद्ध हो जाती हैं। तो युद्ध कौन करेगा । फिर मन का व्यापार वर हुआ इंद्रियों का जो स्वामी है वह मन है और मन ही इन्द्रियों का प्रेरक है। मन के ही कहने सुनने में इन्द्रियां चलती हैं तो सन जब एकाग्र हो गया, मन का निरोध हो गया अर्थात् मन का व्यापार शून्य होने पर इन्द्रियों का भी व्यापार शून्य हो जाता है और इसी को समाधि कहते हैं । जो समाधि निष्ठ पुरुष है, जब ऐसी अवस्था में बोलना-चालना ही बंद हो जाता है तो युद्ध कैसे होगा।
दुकान में बैठे हो सौदा तौल रहे हो, आत्मचिंतन हो रहा है, भोजन कर रहे हो, आत्मचिंतन हो रहा है। क्योंकि हमको सर्वकाल की मर्यादा रखनी है। सर्वकाल में मुझ आत्मा का स्मरण भी कर और युद्ध भी कर । तो फिर किसका चितन? वया लक्षण है ? अरे ! कोई लक्षण नहीं है क्योंकि अलक्षणम् । जत्र में आत्मा अलक्षण हूं ता मुझ आत्मा का चिन्तन भी तो अलक्षण है, भैय्या । और लक्षण वाला चिन्तन हर काल में हो नहीं सकता । भगवान कृष्ण जैसे टेढ़े हैं उसी प्रकार उनका उपदेश भी टेढ़ा है भैय्या । इनको लगाना, भगवान योगेश्वर के इस रहस्य को समझना साधारण नहीं है ।
देखो कौन सा ऐसा टाईम है, कौन सी ऐसी अवस्था है जब में आत्मा न रहूं । अरे ! सबेरे सोकर उठे और करीबन रात दस बजे सोते हैं तो पांच और दस के बीच कोई ऐसा टाईम है जब में आत्मा न रहूँ । पांच और दस के बीच जो टाईम है उसको जाग्रत अवस्था कहते हैं । तो जाग्रत अवस्था के प्रपंच को कौन जानेगा, कौन अनु- । भव करेगा। तो मैं रहता हूँ। 'मैं' आत्मा । सर्वकाल में जो रहने वाला जो आत्मा है उसकी यह अनुभूति कराई जा रही है। चिन्तन श्री बाद में बताया जायगा । तो. जाग्रत में 'में' रहता हूँ और जो 'में' आत्मा जाग्रत अवस्था में रहता हूँ, जाग्रत अवस्था तो बदल जाती है मगर में वही का वही रहता हूँ । यदि माप्त काल में मैं नहीं रहूंगा तो स्वप्न के प्रपंच को कौन जानेगा । श्री में' जाग्रत में और स्वप्न में रहता हूँ वही मैं आरमा गाड़ी निद्रा भुषुप्ति में रहता हूँ। जिस अवस्था में जाग्रत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं का अभाव हो उसको सुषुप्ति कहते हैं। मैं कहाँ पड़ा हूं इसका होश नहीं रहता । जो मैं जाग्रत में वही में स्वप्न में, जो जाग्रत और स्वप्न में वही गाढ़ी निद्रा में रहता हूं । क्योंकि सबेरे'मैं' कहता हूं कि ऐसा सोया कि कुछ पता ही नहीं रहा। अगर में सो जाता तो बताता कौन ? तो मैं सोया नहीं। जाग्रत अवस्था सुषुप्ति अवस्था मन की है। बुद्धि की है। अगर मैं सो जाता तो पता का पता किसको रहता । दूसरी चीज यह है कि कहते हैं कि बड़ा आनंद आया मैं आत्मा वहाँ नहीं रहता तो बड़ा आनन्द आया, इस आनन्द का कौन अनुभव करता । तो इसलिए जाग्रत में, स्वप्न में सुषुप्ति में न रहूँ । स्वप्न में न रहूँ तो स्वप्न प्रपंच को कौन जानेगा। तो तीनों अवस्थाओं में मैं आत्मा एक रस रहता हूँ ।
अब देखो, भूतकाल, भविष्यत् काल और वर्तमान काल । आज के पहले भी 'मैं' था और आगे भी रहूंगा और कभी भी मैं हू। आज के पहले भी मैं आत्मा था, इसका क्या प्रमाण है ? तब इसका हो क्या प्रमाण है कि आज के पहले मैं नहीं था ? अगर 'था' का प्रमाण मांगते हो तो नहीं, था का प्रमाण दो। दूसरी चोज यह है कि जैसे किसी ने कहा- आज के पहले 'मैं' नहीं था। मैं नहीं था। 'मैं' के अभाव को जानने वाला, मैं नहीं था । 'नहीं था' को 'नहीं था' ने जाना, कि 'नहीं था' को 'था' उसने जाना ? जो थर उसने जाना। तो मैं नहीं था इसका अनुभव करने वाला तो'मैं' ही हूँ। मैं के भाव अभाव का ज्ञाता तो मैं 'ही' हूं। जिज्ञासुओ ? भगवान को जानने के लिए, भगवान को देखने के लिए भगवान का अनुभव करने के लिए तुमको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं । डंके की चोट पर, क्यों कि मैं आत्मा वाणी का विषय ही नहीं और वेद शास्त्र, श्रुतिया, स्मृतियां वाणी रूप हैं तो मुझ सत्य आत्मा का प्रमाता ये तो नहीं हो सकते ।
प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् । इत्यादि
जो पदार्थ सत्य सनातन होता है उसकी किसी अन्य प्रमाण से सिद्धि नहीं होती प्रमाता-प्रमाण और प्रयेय तीन चीज़ है। प्रमाता कहते हैं- प्रमाण देने वाले को। जैसे किसी ने पूछा- स्वामी जी के हाथ में क्या है ? तो स्वामी जी के हाथ में जो है वह डण्डा है। तुम हुए प्रमाता । तो सत्य भगवान आत्मा के लिए प्रमाण देने वाला जव प्रमाण देने के लिए आएगा तो सत्य से जो भिन्न होगा वह सत्य होगा कि असत्य ? सत्य से भिन्न असत्य, चेतन से भिन्न जड़, आनन्द से भिन्न दुःख, प्रकाश से भिन्न अंधकार । हां जी । प्रकाश का प्रमाता तो प्रकाश ही होगा । प्रकाश को प्रमाणित करने के लिए किसी और को मानोगे तो प्रकाश से भिन्न होता है अंधकार । अंधकार प्रकाश का प्रमाता तो हो नहीं सकता । सत्य का प्रमाता सत्य ही होता है। तो गरज यह है कि आज से पहले भी मैं था। तो इसका प्रमाता में ही हूं।
कर्म और उपासना फिलासकी जीव जगत की है। सत्य सबका एक हैं। अगर कहो हिन्दुओं का सत्य अलग है, मुसलमानों का सत्य अलग है तो ऐसा नहीं है। जो सत्य है वह सारे विश्व का एक है और सत्य परमात्मा का विवेचन हो रहा है। हिन्दू फिलासफी तो पुनर्जन्म को मानती है, मगर इस्लाम धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता । यह उनका स्वयं का सिद्धांत है। और सत्य की अनुभूति उन्हें भी करानी है। अगर सामने यह दलील रखते हो तो पुनर्जन्म किसका होता ? तो यहां पर मज़हब आ गया । तो यह कर्म फिला. सकी पर रखो । इसलिए इसको प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं । जो यह कहते हैं कि वेदणास्त्र भी तो अपने अपने दिमाग का फुजला निकालते हैं। और में जैसा हूं वैसा ही हूँ। इस- लिए भगवान सत्य परमात्मा को लखने के लिए सत्य ही उसका प्रमाण है। मैं का प्रमाता में ही हूं। प्रकाश को देखने के लिए प्रकाश ही उपकरण है। तो गरज़ यह है कि प्रकाश को प्रमाणित करने के लिए दूसरा नहीं है। प्रकाश को प्रकाश ही देखता है। उसी तरह में आत्मा का प्रमाता में ही हूं। अहम् करके अहम् का ज्ञान होता है। में वाज वक्त कहा करता हूं- मैं ब्रम्ह हूं इस ज्ञान को प्राप्त करते के लिए बुद्धिमान और विद्वान होने की जरूरत है क्योंकि जब तुम्हारी प्रखर बुद्धि होगी । तभी वेदान्त के ग्रंथों को लगा सकते हो तो पहले व्याकरण पढ़ो फिर उसके बाद न्याय शास्त्र पढ़ो । इसके बाद वेदांत पढ़ो । फिर वेदान्त के ग्रंथ तुम्हारी समझ में आ सकते हैं आज कल भी जो कृतियां विद्वानों ने जो संस्कृत में थी, उसका हिन्दी करदिया है- विचार सागर है, वृत्ति प्रभाकर है । तो वेदान्त के ग्रंथों क लगाने के लिए तो बुद्धिमान, विद्वान होने की जरूरत है। प्रब बुद्धि न होगी तब तक वेदान्त के ग्रंथों को लगा नहीं सकते । वेदां के ग्रंथों को पढ़ने से यहां तक वह आता है विद्वान, कि 'में संसा जीव नहीं, शरीर से भिन्न 'मैं' व्यापक ब्रम्ह हूं।' इसी का पठन पाठन होता है। हम सब पापड़ बेले हैं ।
पंजाब में एक फरीद कोट स्थान है। फरीद कोट में एक फक रहते थे उनका नाम था बाबा फरीद । एक दिन उनके साथ मि के लिए एक शायर मियां शेख शादी आए थे ।
मियाँ शेख शादी उनके बैठक खाने में जहां वे एक पलंग पर बैठे हुए थे गये, और उनके सामने फर्श पर जहाँ, वैठने के लिये उन्हें आसन दिया गया था बैठ गये, इसके बाद परस्पर चर्चा होने लगी अचानक, मियां शेख शादी की नजर उनके पलंग के पायों (खूरों) पर गई तो उनके देखा कि उन पायों के नीचे चार बड़ी २ मोटी २ पुस्तकें दढ़ी रखीं हुई हैं। यह देख आश्चर्यचकित हो उनने बाबा फरीद से पूछा, कि फरीद साहब ? पलंग के इन पायों के नीचे आपने ये क्या दबा रखा है ? तब बाबा फरीद ने उन्हें उत्तर दिया कि भाई ! ये हमारे (मुसलमानों के) चारों मुख्य ग्रन्थ हैं (तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान) ये हमें रात-रात भर सोने नहीं देते बड़े शोर मचाते रहते हैं कि ये करो, ये न करो ऐसा है, वैसा है-आदि इनके विधि निषेध के हो हल्ला के मारे हम चैन से सो भी नहीं पाते थे इसलिये इन्हें चारपाई के पायों के नीचे दबा रखा है कि चुपचाप शान्त-दये पड़े रहो तुन्हें शोर मचाने की जरु- रत नहीं। कुछ मत बोलो। जब तक मुर्सद की मेहर नही हुई थी, तब तक किताबों ने मुझे कुछ नहीं बताया और अब, जबकि मुर्शद को मेहर हो चुकी है तब इनकी जरुरत नहीं है। तात्पर्य यह है कि वेद शास्त्र वाणी रूप ही हैं और भगवान आत्मा वाणी से परे है, तब इनकी जब वहां तक पहुँच हो नहीं है तब ऐसी स्थित्ति में इन्का -शोर शराबा वहां पहुँचे हुए "मुकामीजनों" (जो मुकाम पर पहुँच गये हैं) के लिये व्यर्थ ही तो है। वे उनका कब सुनने वाले हैं। हाँ वेद जो हैं व्यर्थ नहीं है। मगर जिनकी बुद्धि में तर्क है वे इसका पठन-पाठन करते हैं और आखिरी इन शास्त्रों के पड़ने का यही रिजल्ट होता है। कि मैं संसारी, जीव नहीं हूँ, व्यापक ब्रह्म हूँ । और यहीं तक वेद शास्त्रों की मर्यादा है और जहाँ पर 'में । जब मैं आत्मा को देखने और अनुभव करने का मौका आता है तो यह सब किनारा काट जाते है। भगवान को जानने के लिए विद्वत्ता और मूर्खता से इसका कोई संबंध नहीं है। अरे यार ! 'में 'हूँ' इसको कौन नहीं जानता ? जो बड़े से बड़ा विद्वान है वह भी 'मैं' हूँ कहता है और जो निरक्षर भट्टाचार्य है वह भी मैं हूँ कहता है। इसलिए उसको जानने के लिए विद्वान होना कोई आवश्यक नहीं है। जानना तो इतना ही है। चाहे जिंदगी भर पढ़ो । खोदने को पहाड़ और निकलने को वुहिया । इसको जानने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। 'में को जानने के लिए में ही साधन हूँ । 'मैं' ही 'मैं' का प्रमाता हूँ। जिसका प्रमाण संसार में कोई न दे सके तो 'मैं' भगवान के सिवाय कौन होगा । भगवान सबका प्रमाता है भगवान सत्य सनातन है और अनन्त है जन्मों से इसी परम तत्त्व को जानने के लिये जो कुछ भी लोग किए हैं आज भी जो कुछ कर रहे हैं आगे जो कुछ करेंगे हर एक की मंजिल मकसूद यही है। जिसका कि अनुभव कराया जा रहा है। गजल
तो भैया ! गरज यह है कि अनन्तकाल से एक ही मंजिल की तरफ सवका बहाव है यानी सभी जा रहे हैं। कोई आज पंहुँचा, कोई कल पहुँचा । मगर सबकी जो आखिरी मंजिल है वह यही है कि में हूँ आत्मा । इसे ही देखना है, इसका ही अनुभव करना है और इसका ही चिन्तन करना है तो भगवान के इस मंत्र की व्याख्या की जा रही है अचिन्त्य पर ।
'तस्मात्, सर्वेषुकालेषु मामनुस्मर युद्ध च ।'
सर्वकाल में मुझ आत्मा का स्मरण भी कर और युद्ध भी कर । सर्वकाल में मुझ आत्मा के सिवाय दूसरा नहीं। अब यहां पर एक प्रश्न होता है जब अस्पताल में आपरेशन होता है और अस्पताल से डाक्टर लोग जब उसको छुटकारा दे देते हैं तो कहते हैं आपका आपरेशन बड़ा सीरियस था तो कहता है भैय्या ! हम तो मौत के मुंह से निकले हैं। तीन घटे तक में बेहोश रहा । क्यों जी; मैं बेहोश हो जाता तो तीन घंटे की बेहोशी का अनुभव कौन करता ? में बेहोश नहीं हुआ । मैं तो होश को भी जानता हूँ और बेहोश को भी जानता हूँ । उस वक्त बेहोशी को इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उस वक्त बेहोशी को बताने का उपकरण नहीं रहता । मगर में ज्यों का त्यों रहता हूँ। मुझ आत्मा में किसी किस्म का परिवर्तन नहीं होता । जाग्रत में, स्वप्न में सुषुप्ति में, भूत में भविष्यत् में और वर्तमान तीनों काल में, हर अवस्था और हर हालत में 'मैं' आत्मा ज्यों का त्यों रहता हूँ। इसीलिए-तस्मात् सर्वेषुकालेषु युद्ध च । अब चिन्तन प्रकरण आया अचिन्त्य का । आत्म चितन का क्या स्वरूप है जबकि श्रुति कह रही है अचिन्त्यम् । तो फिर आत्म चिन्तन का क्या स्वरूप है ? यह तो निविवाद सिद्धांत-है कि सर्व- काल में में ही रहता हूँ तो फिर चिन्तन किसको कहते हैं। मुझ आत्मा के चिन्तन का संबंध चित्त से तो है नहीं । न आँख के बन्द करने से है, न आँख के खोलने से है न किसी अवस्था से है न किसी अचिन्त्य काल से है न किसी देश से है । अब इसका के चिन्तन का यही स्वरूप है। किसी भी प्रकार का चितन न हो। ठीक । में आत्मा हूँ, इसका भी चिन्तन न हो। मैं आत्मा हूँ यह चिन्तन भी चित्त का ही है। चित्त से ही संबंधित है। अब यहाँ पर एक चीज और बताना है। जो-एलाक में अगला शब्द है-'युद्धच' । खाली चिन्तन हो रहता तो कोई बात न थो। मतलब यह है कि सब काम होते हुए भी मुझ आत्मा का स्मरण कर । कथा सुनते हुए भी मुझ आना का चिन्तन कर इसो माण्डू क्योपनिषद में कारिका आती है-
'यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।
निङन मनाभासं निष्पन्नं ब्रम्हतत्सदा ॥४६॥ .
(गौ. पा. कारि. अद्वैत प्र. म. स. ।।४६।।)
भगवान आचार्य कहते हैं-मानो जिस वक्त चित्त का लय न हो और चित्त विक्षिप्त न हो तो लय और विक्षेप से रहित जो अवस्था है वही ब्राह्मी अवस्था है, वही अचल पद है और वही भगवान आत्मा में हूं।
चित्त के लय का क्या स्वरूप है ? और चित्त के विक्षिप्तता का क्या स्वरूप है ? चित्त की चंचलता को चित्त का विक्षेप कहते हैं चंचलता का नाम-विक्षेप है और नींद आ जाना यह चित्त का लय है। अभी इस वक्त चित के लय में सुन रहे हो या चित्त के विक्षेप में सुन रहे हो या लय-विक्षेप दोनों से रहित अवस्था में सुन रहे हो क्योंकि यदि चित्त लय हो जाएगा, तो झोंके लेने लगोगे । और विक्षिप्त हो जाएगा तब भी नहीं सुन सकते और लय विक्षन से रहित अवस्था ही ब्राह्मी अवस्था है।
सशांत सर्व संकल्पा या शिभावद् अवस्थिति ॥
जाग्रन्निद्रा विनोर्मुक्ता सा स्वरूपस्थिति परा ॥
जाग्रत और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं से परे की जो अवस्था वही स्वरूपस्थता है। तो अभी जो सुन रहे हो यह निरूपण तो स्व- रूप में स्थित होकर सुन रहे हो या स्वरूप से बाहर होकर ? स्वरूप में स्थित होकर ही यह निरूपण सुन रहे हो। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं संमार में व्यावहारिक जगत के अन्दर, वे सब स्वरूपस्थता में होते हैं कि स्वरूपस्थता के बाहर ?
तो यही तो भगवान आत्मा का सर्वकाल में स्मरण है। मगर तारीफ यह है कि किसी भी कार्य के क्रियाकाल में यह भी तो चिंतन नहीं होता कि मैं आत्मा हूं और अगर यह चिंतन करो कि में आत्मा हूं, तो मैं 'अचिन्त्य' नहीं। यही तो भगवान आत्मा का स्वरूप है । कि यह भी स्मृति न रहे कि मैं आत्मा हूं। यही आत्म चिन्तन है और अचिन्त्य पद है। श्रुति जो कह रहो है आत्मा अचिन्त्य है । तो क्या मतलब है? अगर पोजीशन बनाकर बैठो तो मैं ऐसा नहीं ।
'नान्तः प्रज्ञं .... ……… सविज्ञेयः
इसी वजह से अचिन्त्य पद में स्थित होकर ही जगत प्रपंच का सारा काम होता है । लय और विक्षेप नहीं तो मन कहां है ? तो अमनस्क पद में स्थित होकर तुम्हारा सारा व्यवहार होता है और विना प्रयास के अमनस्क पद में स्थित होने के लिए क्या तुम कोई साधन करते हो अमनस्क तो तुम स्वयं हो अब हम तुमको किस पद में स्थित कराएं अरे ! तुम खुद अमनस्क पद में तो तुम बिना प्रयास के बिना साधन के स्वाभाविक स्थित हो तो फिर हम क्या करते हैं ? जिसमें तुम हो पहले से उसमें रहो तुम्हारी जो कोशिश है न, उसको हम खतम करते हैं। कोशिश करते थे तब भी वही थे। और कोशिश मत करो तब भी वही हो । मगर तुम्हारा जो विकल्प था कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, बस इसी विकल्प को संत महात्माजन लखाते हैं, जो तुम हो जहाँ पर हो वहीं लखाया जा रहा है और अगर मैं यह विकल्प करू, कि में तुमको अपने पास से कुछ दे रहा हूं तो फिर मैं ब्रम्ह विद्या का प्रवक्ता नहीं हूं, मेरे अंदर पोल ही है फिर । अरे तुम भगवान हो, तुम्हें कौन दे सकता है तो जहां पहले थे, जो थे, अरे जो भगवान है उसको भगवान कहा जायगा या खचेडू को भगवान कहा जायगा? जो वास्तविक चिन्तन है भग- वान का वह यहो है। कि 'मामनुस्मर युद्धच ।
.
अब चार बज रहे हैं, आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है।
ॐ पूर्ण मदः पूर्ण मिद, पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण मेवाव शिष्यते ।।
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! ! शान्तिः ! ! !
पंचम दिवस का प्रवचन
(शुक्रवार, दिनांक १६ नवम्बर सन् १९७३ (समय १० बजे से १२ बजे तक)
ओमित्येत दक्षरमिदꣲ᳭ सर्व………….. तदप्योङ्ग्कार एव ।
नान्तः प्रज्ञम् …………………. सविज्ञेयः
'सोयमात्मा ……………………. मकारति,
आत्म जिज्ञासुओं ? कल के प्रसंग में भगवान स्वरूप आत्मा को महारानी श्रुति ने अचिन्त्य बताया है-
'नान्तः प्रज्ञम्…………………….
यदि में आत्मा अदृष्ट हूँ और अदृष्ट होते हुए अग्राह्य हूँ, अग्राह्य होते हुए अव्यवहार्य हूँ । अव्यवहार्य होते हुए अचिन्त्यम् । मैं आत्मा अचिन्त्य हूँ । अचिन्त्य याने होता है किसी के द्वारा जिसका चिन्तन न किया जा सके उसका नाम अचिन्त्य है। जो मन द्वारा, चित्त द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जिसका चिन्तन न किया जाय उसको अचित्य कहते हैं। तो मैं आत्मा अचिन्त्य हूँ। कुछ लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान में जब कुछ दिखाई देता है, कोई दृश्य, तब तो प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि आज ध्यान में मैंने इस चीज का दर्शन किया । आज हमको प्रकाश दिखाई दिया और अगर कुछ नहीं दिखता तो ध्यानी जो है साधक, उसका निराश होकर मुंह लटक जाता है। आज हमको कुछ दिखाई न दिया । अरे भैय्या ! तुझे देखना ही है तो आंख क्यों बंद करता है। ये बिना कुछ किये ही देख रहा है। तो आंख बंद करके भी वह साधक देखने की कोशिश कर रहा है। तो आश्चर्य ही तो है जो कहता है हमको बड़ा भारी प्रकाश दिखता है। तो प्रकाश hat pi तो दिख ही रहा है। तो वास्तव में ध्यान, ध्यान है। उस ध्यान को ध्यान कहते हैं कि कुछ न कुछ दिखाई दे। न ये शब्द, न स्पर्श' न रूप, न रस, न गंध, यानी भी दिखाई न दे । तो कुछ न दिखने पर, कुछ न दिखाई देने पर, देखने वाला ही तो वहां रहता है और कौन रहेगा ? अरे जब कुछ नहीं दिखता तव मैं तो दिखता हूँ कि में भी नहीं 'दिखता अरे कुछ नहीं दिखना ही तो मैं का दिखना है जिस वक्त कुछ न दिखाई दे ध्यान में, तो कुछ न दिखाई देने पर ये तो अनुभव होता है कि कुछ नहीं दिखता, कुछ दिखता है उसका भी अनुभव करता है ।. और कुछ नहीं दिखता इसका भी अनुभव करता है । दिखने, और न दिखने दोनों को जो देखता है वह तो दिखता है। यही तो पक्का ध्यान है। मगर बिना सोचे समझे लोग निराश हो जाते हैं। जो असली ध्यान है उसकी तो लोग उपेक्षा करते हैं और जो नकली ध्यात है उसकी अपेक्षा करते हैं। जब कुछ नहीं दिखाई देता । सुना विल्कुल। ये भी बता दिया गया है कि अगर तुमको कुछ दिखाई देता है तो मैं का डंडा मारो। कुछ दिखाई देना आत्म चिन्तग का बाधक है । स्वरूप चिन्तन का, आत्म चिन्तन का, ब्रह्म चिन्तन का बाधक हैं। इसलिए जब कुछ खुर्र, खरं मालूम पड़े, विचार, कल्पना या कोई दृश्य तो फट से मैं का डंडा मारो । इसका जो आदर है डंडा लगाओ उसके ऊपर। मार ही दो । तुमको पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसकी अन्यथा सिद्धी है न । फिर शांत मुद्रा में बैठो । आख खुली रहें या बंद रहें। आंख का कोई मतलब नहीं है। न तो ये आंख है, न ये कान है, न ये मुह है। ये सब गोलक है। आंख उसके अन्दर है। विचार दृष्टि से देखो तो इंद्रिय एक ही है-मन । शब्द विषय का भोग करने के लिए ये जो मन है, इस प्रदेश में आता है, तो इसी मन का नाम कर्ण इंद्रिय हो जाती हैं। जब इस प्रदेश मैं - आता है'तो आंख नाम हो जाता है। इंद्रिय देस नहीं है। अगर -इंद्रिय दस हों या पाँचे हों तो एक ही समय में हर एक इंद्रिय अपने अपने विषये को ग्रहण करें। आंख देखने लगती है तो कोन काम नहीं करता। अंगर ये इंद्रियां दस या पाँच है तो फिर एक ही टाईम में जिस इंद्रिय का जो विषय है वह इंद्रिय एक हीं कॉल में अपने- अपने विषयों की ग्रहण करे। मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि मन एक ही है। इसलिए ये तो जीवन भर सुनों हम तुमको सुनायेंगों बढ़िया- बढ़ियाँ चीजें । मगर किसी को शब्द जाले में नहीं फंसाना है क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी है इसलिए वेदांत में हम तीन ही चीज समझातें हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल पदार्थ में शरीर समझ लो । सूक्ष्म में मन संमझ लो और स्थूल सूक्ष्म का कारण जो आत्मा है उसको समझा दिया।
तो भैय्या ! कहने का मतलब यह है कि जिस समय आत्म चिन्तन करने के लिए बैठो तो यह कल्पना तो मैं आत्मा की कल्पना है। सो जिससे जो चीजें पैदा होती है उसी से वो मरती भी है। सर्प बाहर से नहीं आंता इसलिए रस्सी का ज्ञान ही सर्प की मृत्यु है। तो यह सकल्प विकल्प जो भी पैदा होता है उनकी मुझे आत्मा से ही उत्पत्ति है। तो में ही इनका नाशक हूँ। जहां मैं का डंडा लगा, वहीं नाश भी हो जाता है। इसलिए कोई चिंता न करो । शाँत बिलकुल । कुछ देखने का विकल्प न करो कि ध्यान में हमको कुछ दिखाई दे। ये ध्यान नहीं है ये विकल्प है। उस ध्यान काल में ध्यानावस्था में नः शब्द, न स्पर्श न रूप, न रस, न गंध, न देश, न काल, न वस्तु । वस्तुतः यही आत्म चिन्तन है। हालांकि बिना बोध के इस प्रकार के चितन में हरएक की आस्था नहीं हो सकती। क्योंकि अनादि काल से नाम रूप में आस्था जमी हुई है और नाम रूप में मन को रखते हैं तो आँख बंद करके भी नाम रूप देखने के ही कोशिश करते हैं लोग। ये गलत ख्याल हैं। जिस समय आत्म चितन में बैठो उस समय में ध्यान करने बैठा हूँ या "ध्यान कर रहा हूँ। इसका भी चिन्तन न हो क्योंकि में चितन करने बैठा vec R तो ये चिंतन सर्वकाल वाला नहीं है। जो चितन भगवान आत्मा का स्व- भाव में होता है वही सर्वकालीन होता है और जो पर भाव में होता है वह कभी होता है और कभी नहीं होता । तो भगवान आत्मा का चितन सर्वकालीन है और सर्वकालीन होने के ही कारण स्वभाव में होता है । स्वभाव । स्व माने आत्मा के होते है, मैं के । जो चितन आत्मभाव में या में भाव में होता है वही चितन सर्वकालीन होता है। उसो के लिए भगवान ने कहा है- 'सर्व कालेषु मामनुस्मर युद्धच ।
भगवान का वही चितन स्वभाव में होता है परभाव में नहीं होता । अपने आत्मा को कुछ मानकर चिन्तन किया जाय बही पर भाव है। और अपने आप आत्मा को कुछ न मानकर चिंतन किया जाता है उसे स्वभाव का चितन कहते हैं। तो जो स्वाभाविक चितन है भगवान का वही सर्वकाल में हो सकता है। परभाव का जो चितन होता है वो करने से होता है स्वभाव का वितन न करने से होता है । क्योंकि अपने आप को कुछ मानकर चितन करने बैठोगे तो उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आख बन्द करना पड़ेगा. आसन लगाना पड़ेगा, देश-काल ढूढ़ना पड़ेगा, तो परभाव के चितन में कुछ करने की जरूरत होती है और स्वभाव के चितन में- स्वभाव में जो चिंतन होता है बिना कुछ किये है और परभाव का चिंतन करने से होता है। तो बिना कुछ किए जो चिंतन होता है, वही सहज चिंतन है और वही सहजानंद है, वही सहज समाधि है और वही सह्न पद है । जब तक आत्म तत्व का पूर्ण रूप से बोध नहीं हो जाता तबतक स्वभाव का चिंतन असम्भव है। हाँ तो ठीक है। आत्म नैष्ठिक या ब्रम्ह नैष्ठिक का ब्रम्ह चितन अथवा आत्म चितन स्वभाव में होता है। और आत्म वेत्ता या ब्रम्ह वेत्ता का आत्म चितन परिछिन्न होता है । सर्वकालीन नहीं होता। सबसे पहले तुम्हें ये बता देंगे कि आत्म नैष्ठिक किसको कहते हैं, और आत्म वेत्ता किसको कहते है ।
देखो शादियां तो सभी लड़कियों की होती है। चाहे १८ साल में, चाहे २० साल में, चाहे पच्चीस साल में, शादियां तो सभी लड़कियां करती हैं। शायद हजारों में कोई एकाध अविवाहित हो जाय । मगर इन शादी शुदा में पतिव्रता ? होती सभी पति वाली हैं। मगर पतिव्रता कोई-कोई होती है। पतिव्रता के तो दर्शन ही दुर्लभ है ।
'उत्तम के अस-बस मनमाहीं । सपनेहु आन पुरुष जगनाहीं ।'
चाहे पति कुरूप हो, रूपवान हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, या दरिद्र हो। आरोग्य हो या रोगी हो- मगर 'सपनेहूं आन पुरुष जग नाहीं' पतिव्रता के समक्ष (विष्णु भगवान भुवन सुन्दर कहे जाते है) कोई भी सामने आ जाय तो पतिव्रता उनके तरफ भी दृष्टि उठाकर नहीं देखती । आ, हा-हा ? वैसे सभी पति वाली हैं। सात भांवर सबके साथ पड़ती है। पतिव्रता का दर्शन ही दुर्लभ है। चाहे पति नैष्ठिक कहलो । उसी तरह बोध हो जाना दूसरी बात है। जान लिया मैं आत्मा हूँ. मैं व्यापक हूं, अखण्ड हूँ । बोध हो गया है लेकिन भगवान आत्मा के प्रति निष्ठा हो जाना, दूसरी बात है। ब्रह्म को जान लिया उसका नाम हुआ ब्रह्मवेत्ता और स्वरूप आत्मा में निष्ठा हो जाय उसको कहते हैं ब्रह्म नैष्ठिक या आत्म नैष्ठिक । ब्रम्ह नैष्ठिक तो शायद ही कोई मिले । नैष्ठिक नहीं मिलते । जो ब्रह्म नैष्ठिक होता है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण सुन्दर से सुन्दर कहे जाते हैं मगर पतिव्रता उनके तरफ नहीं देखती उनी तरह आत्म नैष्ठिक जो पुरुष है तो दुनियां की दृष्टि में उसके लिए न कोई देवी न कोई देवता । और ब्रम्हा, विष्णु, शंकरादिक के भी चमत्कार देखकर उसका चित्त विचलित नहीं होता । उसको आत्म नैष्ठिक कहते हैं। ये बात नहीं है कि बीज नाश हो जाय, लेकिन बाजार नहीं है उनका। जो आत्म नैष्ठिक का चिंतन है- वह करता नहीं, होता है। और जो चिंतन होता है वो होता है स्वाभाविक । बिना किये होता रहता है। इस पर विश्वास जमना एकाएक नितांत असम्भव है । अरे भाई- आत्म नैष्ठिक याने भगवान । आत्म नैष्ठिक कह लो चाहे भगवान । क्या भगवान भी अपने आप से भिन्न देखता है किसी को ? तो स्वाभाविक चितन । स्वभाव में चितन । 'स्वभाव', यह चिंतन । सुनो ! अब इसका अनुभव करो । कल भी इस पर थोड़ी रोशनी डाली गई थी । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गध । ये पाँच हो विषय कहे जाते हैं। जितने विषय हैं इनमें से किसी विषय का भी अनुभव करता हूं। तो भैय्या, परभाव में अनुभव करता हूँ कि स्वभाव में करता हूं ? स्वभाव में । अरे भाई अभो जो कथा सुन रहे हो वो स्वभाव में कि परभाव में ? स्वभाव में । क्या प्रमाण ? विषयों के अनुभव काल में कत्र्ता, क्रिया, कर्म तीनों की अनूभूति होती है तो वह परभाव है। और यदि कर्ता, कर्म, क्रिया तीना की अनूभूति का अभाव है, तो समझना स्वभाव है। यही परभाव और स्वभाव का लक्षण है। और यह लक्षण अकाट्य है। परभाव और स्वभाव का । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध । और इन्हीं पाँचों विषयों क्ता अनुभव होता है । इन्हें चाहे संसार कहो चाहे, प्रपंच कहो, माया कहो । जो मर्जी आये कह लो । बस ये पांच विषय हैं और इन्ही पांच विषयों के अस्तित्व में इन्द्रियों का अस्तित्व निहित है। पहले विषय का विकल्प होता है। जब विषय का विकल्प होता है तो उस विषय का ग्रहण करने के लिए इन्द्रिय पैदा हो जाती है। पहले इन्द्रिय नहीं रहती । इसका निपटारा बाद में करेंगे ।
विषयों के अनुभव काल में यदि कर्ता, कर्म, क्रिया की अनुभूति होती है तो वो परभाव है। और अनुभव काल में कर्ता, कर्म, क्रिया इन तीनों की अनुभूति नहीं होती तो वह स्वभाव है। अब कर्त्ता, कर्म, क्रिया किसको कहते हैं ? कर्ता, कर्म, क्रिया जो देखता है उसको कर्ता कहते हैं और जो चीज देखी जाती है उसको कर्म कहते हैं और जो देखना है वो क्रिया । जैसे अब ये डण्डा देख रहे हो तो तुम देखने वाले हुए कर्ता, डण्डा हुआ कर्म और तुम्हारा देखना हुआ क्रिया । तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच विषय हैं। और हर एक में तीन चीजें रहती है। कर्ता, कर्म, क्रिया । तो जिस तक्त शब्द का स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, तो किसी भी विषय का मैं आत्मा अनुभव करता हूं। मैं याने में, मैं याने तू नहीं। क्योंकि मैं आत्मा सब में ही हूं। मैं तो सब कुछ हूं। जिस समय किसी भी विषय का अनुभव करता हूं तो विषय के अनुभव काल में यह अनुभव नहीं होता कि में देख रहा हूं। ये फर्जी चीज है। कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों के अभाव का जो भाव है वही स्वभाव है तो किसी विषय के अनुभव काल में मुझ भगवान आत्मा को यह अनुभव नहीं होता कि ये अमुक विषय है और में अनुभव करने वाला हूं या इस विषय का में अनुभव कर रहा हूं। कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों भावों का अभाव रहता है। ये तीनो भाव का अभाव ही तो स्वभाव है। वस्तुतः यही आत्म चितन । कोई काम छोड़कर याने सुनना छोड़कर, देखना छोड़कर, याने कोई काम छोड़कर जो चितन है ये सर्वकालीन भगवान आत्मा का चितन नहीं है। ये पर भाव का चितन है। बहुत वारीक चीज है ये । “आनन्द मानन्द करम प्रसन्नम" वाह ! तो फिर कर्ता, कर्म, क्रिया जब तीनो भावों का अभाव हो गया तो तीनों भावों के अभाव के बाद कौन रहा ? स्व का भाव रह गया । तो पर भाव में कुछ हो रहा है कि स्वभाव में । और कर्ता, कर्म, क्रिया जब में परभाव है, और कर्ता, कर्म, क्रिया के भावों में कुछ हो रहा है । व्यवहार । कर्ता, कर्म, क्रिया का जब विकल्प होगा तभी तो कुछ हो रहा है, ऐसा करेंगे और कर्ता, कर्म, क्रिया इन तीनों विकल्पों का अभाव रहता है विषयानुभव में । तो मैं अनुभव कर रहा हूं ये भाव रहता है न ? तो फिर क्या हल हुआ । मैं आत्म चितन कर रहा हूं ऐसा है ही नहीं । अभी तो तुम्हें पक्का करना है न । विषय कितने है ? पांच शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध । इन्ही को प्रपंच कहते हैं और इन्ही विषयों का ही विषय करने का नाम व्यवहार । तो भय्या ! किसी विषय के अनुभव काल में या किसी विषय के विषय काल में ऐसा अनुभव होता है कि में सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ये अनुभव नहीं होता। याने कर्ता, कर्म, किया तीनों का उस समय अभाव रहता है जब तीनों का अभाव रहता है तो भाव किसका रहता है? में आत्मा का । उसी भाव का नाम हो गया स्वरूप । मैं का भाव रह गया आत्मभाव ! और आत्म भाव में याने आत्म देश में कर्ता, कर्म, क्रिमा तीनों का लेश नहीं है। सर्वथा अभाव है अगर उस समय किसी विषय के अनुभव काल में में आत्मा न रहें तब तो कर्ता, कर्म, क्रिया का अनुभव हो । स्वभाव न रहे तब तो कर्ता, कर्म, क्रिया रहे । तो उस समय स्वभाव रहता है। स्वभाव में यह निश्चय है कि कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों का अभाव हो जाता है।
जब तीनों भावों का अभाव हो जाता है स्वभाव देश में, तो फिर देखना, सुनना, बोलना, चलना, उठना, बैठना ये व्यवहार ही कहाँ है ? इसलिए प्रशांत महासागर लहरा रहा है। लगाओ गोता उसमें, तो फिर क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ या तुम कुछ सुन रहे हो ? हो गया फिर । इस स्वभाविक पद में सचित प्रारब्ध क्रियमाण का उन्मूलन हो जाता है। इसकी अनूभूति में सब गया । खत्म । न पुण्य कर्म न पाप कर्म । जब कर्मों का उन्मूलन हो गया तो न स्वर्ग लोक, न नरक लोक, व चंद्र लोक न सूर्य लोक । ये आखिरी पद है। और भैय्या, जब तक होने का अस्तित्व है, पर भाव है। और जब तक होने का अस्तित्व है तो तुम अपने घर में रहो कि मैं आत्मा अजन्मा ब्रह्म हूँ। मगर कर्म अपने देश में है तो, कर्म दिख नन्हा है। अभी नहीं गया। घर में बैठो । नहीं गया । तो उसी वक्त कमों का उन्मूलन होता है-हुआ ही नहीं तीनकाल में जब हुआ नहीं तीनकाल में । जब हुआ नहीं तो किया किसने फिर ? किसी ने नही। परभाव में तो होता है। अरे यार ! कर्म करने वाले अपने आपको कुछ मानकर ही तो कर्म करते हैं न । चाहे अपने को साढ़े तीन हाथ का देह मानकर करें, चाहे संसारी जीव मानकर करें मगर मानकर ही तो करते है। क्योकि कर्म कांडी देहात्मवादी होता है अपने को देह मानकर कर्म करता है और अपने को में जीव है। मानकर उपासना करता है। तो बिना माने कर्म उपासना हो है। नहीं सकते । तो परभाव हो तो है न, और स्वदेश में कोई न रहा। सब उन्मूलन हो गया कर्मो का, न सुख रहा न दुख रहा ।
'पुण्य पाप जब दोऊ नाशै । तब नर मम पुर पावै बासे ॥'
पुण्य, पाप, बांध्यो जगत, को काटन समरथ्थ । ऐसा ज्ञान विवेक है। ये सब अपने हत्थ ।' तो में हूँ, अपने आपको कुछ मानकर कहते हो तो कुछ हो रहा है और स्व को जानकर कुछ नहीं हो रहा है। तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो चिंतन कहाँ हो रहा है। इसीलिए तो में आत्मा अचिन्त्य हूँ । चिन्तन भी तो एक होना ही है। पर- भाव और स्वभाव । तो परभाव में तो होता है। विकल्प देखने- सुनने का । यह विकल्प परभाव से होता है मगर जब अनुभव करने चलता हूँ तो परभाव न रहकर मैं म्वभाव में आ जाता हूँ। इस प्रकार 'आनंद मानंद करम प्रसन्नम्' हो गया । तभी तो बाबा ज खा गये । मनो से मालपूवा । यहां सिद्धान्त तो है। सुनादें फिर ।
एक बार गोपियों ने किसी शुभ पर्व में महात्मा दुर्वासा के पूज के निमित्त अच्छे-अच्छे स्वादिष्ठ पकवान बनाया और यमुना उस पार उनके आश्रम में जाने के लिये तैयार हुईं, परन्तु यमुन में भयंकर पूर था, तब उन लोगों ने भगवान कृष्ण से कहा-भगवन हम लोग महात्मा दुर्वासा के पूजन के निमित्त उनके आश्रम में जा चाहती हैं, परन्तु यमुना में पूर है, इस कारण हम वहाँ जा सकते असमर्थ हो रही हैं, कृपाकर हमें वहां जा सकने का कुछ उपाय बताइये, ताकि हम लोग वहाँ जाकर उनकी पूजा कर सकें इस पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम लोग, यमुना के पास जाकर कहना, कि यदि कृष्ण बालब्रह्मचारी हों, तो ऐ यमुने ! हमें उस पार जाने के लिये मार्ग दे दो ।
यदि कृष्णो बालयतिः सर्वदोष विजितः ।
तर्णिनों देहि मार्ग बै, कालिन्दै सरिताम्बरै ॥
तुम लोग इस मंत्र के बल से उस पार जा सकती हो गोपियों ने जाकर यमुना से यही मंत्र कहा, यमुना ने गोपियों को उस पार जाने के लिये मार्ग दे दिया अर्थात इस किनारे से उस किनारे तक जल विहीन पगडण्डी बन गई, जिस पर चलकर गोपियां उस पार चली गई, इसके बाद यमुना फिर ज्यों की त्यों हो गई ।
गोपियों ने उस पार पहुंचकर, महात्मा दुर्वासा के आश्रम में उनकी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजा की, और उन्हें मनों स्वादिष्ठ पकवान का भोजन कराया, बाबा जी ने खूब जी खोलकर भोजन सकिया, पूरे साल गटक गये, गोपियों के लिये प्रसाद तक न छोड़ा । अयह सब कार्य पूरा हो जाने के बाद गोपियां वापस आने को तैयार हुई तब उनने महात्मा दुर्वासा से कहा-महाराज! हम लोग वापस नाना चाहती है, यमुना में भारी पूर है, कृपा कर हमें उस पार जाने के लिये कोई उपाय सुझाइये ।
दुर्वासा ने कहा तुम लोग आई किस तरह से हो ? गोपियों ने कहा-भगवन ! भगवान कृष्ण ने एक मंत्र बताया या उसी मंत्र के बल पर हम लोग यहाँ आई हैं।
महात्मा ने पूछा-वह कौन सा मंत्र था ?
तब गोपियों ने कहा-वह मंत्र था-
यदि कृष्णो बालयतिः, सर्वदोष विजितः ।
तणिनों देहि मार्ग बै, कालिन्दै सरिताम्बरै ।
तब महात्मा ने कहा अच्छा तो अब तुम लोग यमुना से हमारा यह मंत्र कहना कि यदि महात्मा दुर्वासा अभी कुछ भी न खाये हो, एक टुकड़ा भी न छुए हों, तो ऐ यमुने । हमें उस पर जाने को मार्ग दे दो ।
गोपियों ने यमुना के पास आकर यही कहा और तुरन्त यमुना ने उन्हें उस पार जाने को मार्ग दे दिया, गोपियां इस पार आ गई। गोपियाँ जाते समय तो महात्मा के पूजन के ध्यान में मग्न थी, अतः उनके मन में कोई विचार पैदा नहीं हुआ, परन्तु अब वे, इस पार आकर सिर में हाथ रखकर बैठ गई, और विचार कर आपस में कहने लगी, देखो, झूठों का बाजार कैसा गरम है, भगवान कृष्ण झूठे, जिनकी १६१०८ रानियां और एक एक से दस दस पुत्र हैं वे बाल ब्रह्मचारी बनें हैं।
महात्मा दुर्वासा झूझे, जिनने अभी अभी हमारे सामने, मनों से मालपुवा और हलुवा गटक लिया, हम लोगों के लिये प्रसाद तक नहीं छोड़ा, वे कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं खाया, और यह निगोड़ी यभुना भी झूठी, जो इन दोनों की (साक्षी) गवाही दे रही है, इस तरह वे विचारों में तल्लीन हो गई ।
भगवान का वास्तविक रूप, यह जो भास रहा है। नाम लिय कि प्रपंच खड़ा हो जायेगा । ये भगवान का आधिभौतिक रूप है।
'हम सकल होने के नाते, हम सकल जो कुछ भी है। खुद सिवा जब कुछ नहीं, संसार कहना जुर्म है ॥ तो भैय्या, ये भगवान की आधिभौतिक रूप है। राम, कुष्णादि भगवान का आधि दैविक रूप है। याने रज वीर्य का शरीर नहीं माना जाता । इच्छामय । और तुम्हारा तो स्वरूप, भगवान आत्मा का, निरूपण किया जा रहा है। यह भगवान का वास्तविक रूप है। यह सारे चराचर को धारण कर रखा है। तो गोपियां भगवान कृष्ण के आधिदैविक रूप की उपासिका थीं। भगवान के वास्तविक स्वरूप का उन्हें ज्ञान नहीं था। गोपियों को जब स्वरूप ज्ञान हुआ तब ये रहस्य समझीं कि भगवान कृष्ण बाल ब्रम्हचारी हैं। तो आत्म देश में तो कुछ हो हो नहीं रहा है। न में कुछ बोल रहा हूं न तुम सुन रहे हो। तो परभाव और स्वभाव का विवेचन हो रहा है। कथा सुनने के लिये जब तुम घर से चले हो तब परभाव को लेकर चले हो सूनूंगा, ये विकल्प लेकर । और यहां बैठे तब भी श्रोता बनकर और सुनने का मौका आया तो परभाव निकल गया । अव स्वभाव में बैठे हो । और जब कथा बंद हुई तो किसी ने पूछा- कि क्या सुने ? तो पहले वाला विकल्प फिर आ गया और जो विकल्प जी-जी के मरता है स्वभाव में तो मर जाता है अरे जो जी-जीकर मरे वो परभाव है और जो न जीये, न मरै वो स्वभाव है। मतलब की बात होती है तो जी जाता है। जितने बहरे होते हैं। वो बड़े मतलबी होते हैं उसके मतलब की बात कहो तो धीरे से भी कहो तो सुन लेंगे । अगर उसके मतलब की बात नहीं है तो फिर बहरे वन जाते हैं ।
तो जो जी-जी के मरे वो परभाव है और जो कभी न जीये न मरे वो स्वभाव है ।
"स्वभावे ब्रम्ह ब्रम्हणि-योऽसि सोऽसि स्थिरोभव"
अरे जैसे हो वैसे ही रहो । 'पर' मत बनो। स्व तो हो ही आनन्द का जब अनुभव करते हो तो स्वभाव में ही करते ही आनंद का जो अनुभव होता है तो स्वभाव में ही होता है। परभाव में आनन्द की अनुभूति नहीं होती। देखो। अब स्वभाव में स्वभावावस्था होकर सुन रहे हो । स्वभाव में स्वभावावस्था होकर देख रहे हो। सारे व्यवहार तुम्हारे स्वभाव में ही होते हैं। मगर उस वक्त ये भी तो अनुभव नहीं होता कि में आत्मा हूं।
'जिसको तुम भूल गये, उसकी याद कौन करे ।
और जिसको तुम याद हो वह और किसे याद करे ।'
और में हूं ये याद है कि नहीं तुमको । तो इसका चितन करने की क्या जरूरत है। जिसको तुम याद हो और किसे याद करे ।
तो में आत्मा हूं। स्वभाव का क्या मतलब । में अमुक हूं ये परभाव, और मैं हूं, ये स्वभाव है। मगर किसी भी विषय के अनु- भव काल में मैं हूं इसकी भी याद नहीं रहती । सिर्फ स्वभाव हो स्वभाव रह जाता है। अच्छा । जब स्वभाव ही स्वभाव रह जाता है तो फिर स्वभाव के सिवाय क्या मन भाव रहता है । मनभाव, चित्तभाव, अहंकारभाव, देहभाव, जीवभाव, आत्मभाव, परमात्मा- भाव । संसार रूपी बाजार के जितने भाव है। उन सब भावों का अभाव हो जाता है। तो ये स्थिति क्या तुमको बनानी पड़ती है ? और ये भगवान श्री कृष्ण क्यों कहते है :-
'तस्मात् सर्वेषु, कालेषु मामनुस्मर'
ये जो स्वभावतः है बिना प्रयास के सबको सिद्ध है। सबको करतल गत है। बस । यही महात्मागण लखाते हैं। इसकी अनुभूति कराते हैं जिसके चिंतन में सिर पर बोझा लगे, किकर पैदा हो जिसके चितन में, वह भगवान का चितन नहीं है। वह पर का चितन है। - जिसके चिन्तन में सिर हल्का हो जाय। किसी किस्त का भार न रहे. हकीकत में वही भगवान का चिन्तन है।
ये फिकर लगी रहती है- अभ्यास में बैठना है। चितन करना है। स्वामी जी? हां जी, तुम तो सब नष्ट करने आये हो, भैय्या ! अपना तो नष्ट हम कर ही दिये हैं। तो तुम क्यों छूटो फिर । अभी तो में फिकर से उठता था चार बजे अब तुम सब के सब का बठाधार करने आये हो । कहते हो फिकर ही न करो। हां फिर ताकत है तो ग्रहण करो फिर हमारे उपदेश को । है किसी की ताकत कि कुछ न करे ? और लोग उपदेश करते हैं, सब कोई, करें ! और हम उप- देश करते हैं- कोई-कोई करें। हमने तो कह दिया परभाव जी-जी के मरता है। तो भैय्या ! साधु-सन्यासी, गृहस्थ-विरक्त सबका यही उपदेश है । सबरे नहा-धोके दो घंटे भगवान का ध्यान करना चाहिए । इसको मानने के लिए सत्र तैयार हो जाते हैं। क्योकि जानते हैं कि बिना कष्ट किए भगवान नहीं मिलता और जो हम कहते हैं, न करने को तो कोई नहीं मानना । कोई-कोई शायद तैयार हो जाय ।
क्योंकि, बिना कुछ किये भगवान नहीं मिलता ये जीव का विकल्प है कि भगवान का । क्या भगवान भी कुछ करता है ? तो हम तुमको आस्तिक बनाने आए हैं कि नास्तिक । पडिताइन जैसी उल्टी खोपड़ी है।
एक स्त्री थी, वह हमेशा अपने पति की आज्ञा के प्रतिकूल कार्य किया करती थी, पति जिस काम को करने के लिये मना करता, वह उसे अवश्य करती ।
एक दिन नदी में पूर था, पतिदेव ने स्त्री से कहा- आज घर ही में स्नान कर लो, क्योंकि नदी में पूर है, वहां नहाने जाना खतरे से पूर्ण है।
पति की बात सुनते ही उसने अपने कपड़े उठाये और वह नदी की ओर चल पड़ी । स्त्री को जाते देख बेचारा पति निराश पूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहने लगा- जाती ही हो तो वहां घाट में पत्थर पर बैठकर ही स्नान कर लेना, पानी के भीतर, कमर तक या गले तक पानी में नहाने मत उतरना । बस फिर क्या था, स्त्री नदी में गई और गले तक पानी में नहाने जाकर पूर में वह गई। लोगों ने जाकर उसके पतिदेव को इस घटना की सूचना दी वह तुरन्त बांस लेकर घाट पर दौड़ा आया और लोगों से पूछा कि भाई ! वह कहां पर डूबी है ?
लोगों ने बताया कि घाट पर पत्थर से आगे पन्द्रह बीस कदम दूर । उस मनुष्य ने डूबने के स्थान से ऊपर चढ़ाव की ओर अपनो स्त्री को खोजना शुरू किया। लोगों ने कहा- भाई ! इधर ऊपर की ओर उसे क्या खोज रहे हो, वह डूबने के बाद तो नदी की बहाव अर्थात् नीचे की ओर ही जायगी, अतः नीचे बहाब को ओर खोजो । इस पर पति महोदय बोल उठे- भैय्या ! तुम लोग इसका रहस्य नहीं समझ सकते, यह स्त्री बड़ी उल्टी गति वाली थी, सीधापन तो इसके स्वभाव में था ही नहीं, सदैव उल्टा ही उल्टा काम किया करती थी, अतः वह डूबने के बाद नीचे की ओर जैसा कि उसे सचमुच ही जाना चाहिये, नहीं गई होगी, वह ऊपर ही मिल सकती है। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि आत्म चितन के लिए कुछ मत करो। बशर्ते कि उसको अच्छी तरह से जान लो । जब तक तुम्हारी जीव धारणा है तब तक बंद हो ही नहीं सकता। क्योंकि जीव की इज्जत इसी में है कि कुछ न कुछ करता रहे । जीव को अगर जिन्दा - रखना चाहो तो करो। करना ही तो जीव की जिन्दगी है और न - किया तो जीव की मृत्यु है। न करने से जीव मर जाता है और न - करने से भगवान हो जाता है। अब जो साइड तुम्हें पसन्द हो चुन लो। अगर जीव बनने में सुख हो जिसके साक्षी तुम स्वयं हो। और भगवान होने में सुख है- शांति है तो भगवान तो हो ही तुम ।
स्वामी जी ! एक शंका और दूर करो। अगर इस बात को ग्रहण कर लिया जाय जो तुम बता रहे हो ? तो इससे बड़े-बड़े अनर्थ भी हो सकते हैं । बुरे काम भी हो सकते है इससे तो। क्योंकि तुम कहते हो स्वभाव में सारे कर्म होते हैं। सारी क्रियाएं होती हैं और स्वभाव में होते हुए भी नहीं हो रही हैं तो करने से बुरा काम भी हो सकता है ।
भैय्या ! पहले इस बोध को प्राप्त कर लो फिर बुरा काम करने का संकल्प उठे तब हमारे पास शिकायत करना । अरे, जब जीव बुरे काम से डस्ता है तो भगवान होकर बुरा काम करेगा ? ये शंका कहां से हो रही है ? जीव देश से । अरे ! जो साक्षात् नारायण है उससे कभी अनैतिक कार्य होगा, उसे विकल्प होगा कि मैं बुरा काम करू ? ये गलत ख्याल है तुम्हारा । इसलिये भगवान अचिन्त्य है उसके चिन्तन के लिए कोई देश काल की जरूरत नहीं है। इसी अचिन्त्य के चिन्तन का नाम अमनस्क पद है।
गज़ल
पी लिया गर जाम तो, फिर याद करना जुर्म है।
कब्र में पड़कर के चीखै, मारना फिर जुर्म है। १।
सोचना था पहिले ही, होना था जो कुछ हो चुका ।
कट गया गर सर जमीं पर, देखना फिर जुर्म है। २।
दो जख बहिश्तों का ए नक्शा देखना तू बद कर ।
वे गुनाह, गुनाहों के, चक्कर में पड़ना जर्म है । '३।
जिन्दगी कश्ती ए दरिया, पार हो हरगिज न हो ।
होकरके बेपरवाह फिर, परवाह करना जर्म है । ४।
हम शकल होने के नाते, हम शकल जो कुछ भी है।
खुद सिवा जव कुछ नही, संसार कहना जुर्म है ।५।
खुद बिना हस्ती खुदा की, कभी टिक सकती नहीं ।
खुद खुदा दो मुखतलिफ, ऐसा समझना जुर्म है। ६ ।
दिल रुबा है जबकि दिल का, और में दिल का सकून ।
वजीरे आजम दिल है मेरा, रोकना फिर जुर्म है । ७ ।
कानून ए पैगाम' 'मुक्ता' को फकीरों से मिला ।
अमल करना है सभी को, ग न करना जुर्म है। ८ ।
अब बारह बज रहे है, मध्यावकाश के बाद दो बजे से प्रवचन पुनः प्रारम्भ होगा ।
शुक्रवार दिनांक १६ नवम्बर सन १९७३
समय- २ बजे से ४ बजे तक
भगवान आत्मा का विशेवण श्रुति ने अचिन्त्य दिया है जिसका विवेचन कल से हो रहा है। अचिन्त्य पद को अमनस्क पद भी कहते है। बिचार वे करना है कि किसी विषय के शब्द, स्वर्ण, सय, रस, वा में जो विषय हैं, इनमें से किसी विषय के अनुभव काल में कर्ता, कई, क्रिया तीनों की अनुभूति नहीं होती । इसका कारण वे है- । बेहया कर्ता, कर्म, क्रिया ये तोनों ही मन कल्पित हैं। और किसी विषय के अनुभव काल में मन रहता नहीं, अमनस्क स्थिति रहती है। यानी सर्वथा विषयानुभूति काल में अमनस्क स्थिति होने के हो कारण कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों की अनुभूति नहीं होती । क्योंकि यदि मन रहे, विषय के अनुभवकाल में तब तो कर्ता, कर्म, किया तीनों का अनुभव हो क्योंकि तीनों की कल्पना मन ने हो तो किया है। अच्छा । तो मन नहीं रहता । अमनस्क स्थिति रहती है। क्यों नहीं रहता ? अब ये दूसरा प्रश्न है। इसलिए कि मन तो परभाव में पैदा होता है । स्वभाव में, आत्मभाव में तो मन नाम की चीज हो नहीं है। कोई न कोई साधन करने से मन अमन नहीं होता, मन निरोध होता है। साधन करने में मन का निरोध होता है अथवा मन का लय होता है- क्योंकि -
नादानुसंधान में मन का लय बताया है। चित्त का तय करने के लिए नादानुसंधान से बढ़कर कोई साधन नहीं है। साधन करने से साधनों से या तो सत्त का विरोध होता है या कोई ऐसा साधन है जिनके करने से मन लय होता है मगर अब अमन नहीं होता। अमन कहते हैं, मन का अस्तित्व हो खतम हो जाय । मन का बजद हो मिट जाय इसको अमन पद या अमनस्क पद कहते हैं। अमन कहते है आत्मा को । मुझ आत्म देश म गन नाम की कोई चीज ही नहीं। जब मन नहीं तो मन द्वारा कल्पित जो प्रपंच है वह भी मुझे आत्म देश में नहीं है इसलिये इसको अमनस्क पद कहते हैं।
क्योकि मन अमन करने का साधन नहीं है। मन के निरोध का साधन है और मन के लय का साधन है परन्तु मन को अमन करने का साधन नहीं है। मन तो उसी समय अमन होता है जहां अपने स्वरूप में स्थित हुआ तो मन अपने आप अमन हो जाता है। स्त्ररू- पस्थ होने पर मन अमन हो जाता है। अच्छा ! अब स्वरूपस्थ कब होता है ? इस प्रश्न से यह मालूम होता है कि क्या स्वरूपस्थ नहीं रहता ? नहीं, स्वरूपस्थ तो रहता ही है। स्वरूपस्थ है ही । सारा चराचर स्वरूपस्थ है। मगर स्वरूपस्थता का अनुभव कब होता है ? ऐसा कहो । स्वरूपस्थ होते हुए भी स्वरूपस्थता की अनुभूति नहीं होती क्योंकि सभी स्वरूपस्थ है। स्वरूपस्थता का अनुभव करने के ही लिए मन को अमन किया जाता है। स्वरूपस्थता का हो अनुभव करने के लिए बिना जाने समझे लोग मन का निरोध करते हैं। योगदर्शन में सूत्र आता है-
योगश्चित्तवृत्ति निरोधः । अभ्यास वैराग्याभ्यां तस्त्रिरोधः ।
मन का निरोध क्यों किया जाय ? तो योग दर्शनकार कहते हैं "तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्"
मन का जो द्रष्टा है उसको स्वरूप में स्थान मिल जाता है। मन का निरोध हो जाने पर साधक को, मन का जो द्रष्टा है, उस द्रष्टा के स्वरूप में साधक को स्थान मिल जाता है, माने इसकी अनुभूति हो जाती है मन के द्रष्टा को, इसलिए मन का निरोध किया जाथ । तो इस कथन से यह सिद्ध होता है कि स्वरूप में स्थित होने के लिए मन का निरोध किया जाता है। मन के निरोध का विकल्प यानी कल्पना प्ररभाव में होती है या स्वभाव में ? मन का में निरोध करू ? जब मैं अपने आपको जीव मानता हूं तभी ये विकल्प उठता है कि मन का निरोध करू । तो गोया मन के निरोध का जो विकल्प है वो भी स्वभाव का नहीं है, परभाव का है। तो अब ये समझना है कि स्वरूप में तो मैं पहले से ही स्थित हूं। स्वरुपस्थ तो मै पहले से ही हूं। अब क्या प्रमाण है कि में स्वरुपस्थ हूं । परन्तु स्वरुपस्थ में नहीं हू यानी स्वरुपस्थता के अज्ञान में ही तो स्वरुप में स्थित होने का विकल्प निहित होता है । य श्रृंखला समझ में आ गई न ? अब गुनो ! इस वजह से मन के निरोध करने का विकल्प होता है। साधन से । देखो भैय्या ! यों तो प्रकृति ने 'मुक्त' को सारे विश्व के कोने कोने में तत्व का प्रचार करने के लिए पैदा किया है परन्तु खास छत्तीसगढ़ में इसलिए भेजा है कि यह बड़ा आलसी देश है। पचास वर्ष के करीब हो गये यार तुम्हारे यहां विचरते। पंजाब ऐसा पुरषार्थी और छत्तीसगढ़ के ऐसा आलसी कहीं न पावोगे । यहां पर एक गाड़ा धान किसी के यहां हो जाय तो राष्ट्रपति हो जाता है। अगर कोई हजारों में एक आध पुरषार्थी निकल आता है छत्तीसगढ़ में तो वो सिद्धान्त नहीं है, अपवाद है। बड़ा आलसी देश है। भगव न के भरोसे बीज फेंक देते हैं खेत में, पानी बरस गया तो ठीक है, नहीं तो हरिहर है। तो कुदरत ने सोचा-अगर साधन बताने वाले महात्मा को छत्तीसगढ़ भेजेंगे तो कर न सकेंगे। तो ऐसे को भेजना चाहिए जो आलस्य धुरीण पद का प्रवक्ता हो उसको इस प्रदेश में भेजना चाहिए । क्योंकि कुछ करने को तो बताते नहीं है। और करने वाला यहां है नहीं । मजा करो फिर क्या है ?
व्यापारे खिद्यतेयस्तु निमेषोन्मेषयोरपि ।
तस्पालस्य धुरीणस्य सुखनान्यस्य कश्चन ।॥
आंख के खोलने और बंद करने का जो व्यापार है, तो श्रुति कहती है आंख के खोलने और बंद करने में भी जिसको थकावट मालूम पड़े, ऐसा जो आलस्य घुरीण पुरुष है संसार में वही सुखी है। तो ये लोग आलस्य धुरीण हैं। कुछ नहीं करना धरना, बस थोड़ा सा धान पैदा हो गया । साल के साल नौकर छोड़ देता है। शायद वैशाख में बैठ जाता है। तो बड़े-बड़े बाबुओं को हमने देखा है। नौकर जब सोया रहता है तो उसके पीछे खड़े होते हैं और जगाते हैं-खेदू, बैसाखू ? बोलता ही नहीं है। क्योंकि पा गया हैं न, आलस्य धुरीण पद । तो भगवान ने सोचा, प्रकृति ने सोचा, कि हम दूसरे साधू को यहां भेजेंगे तो ये काम नहीं होगा । तो ऐसे महात्मा को भेजा जाए जो आलस्य धुरीण पद का प्रवक्ता हो । क्योंकि हम कहते हैं। कि मन का निरोध मत करो क्योकि तुम्हारा किया वह होगा नहीं।
तो मन के निरोध में मन अमन नहीं होता, मन बना रहता है। साधन द्वारा मन का जो निरोध किया जाता है उसमें मन का अस्तित्व खतम नहीं होता । साधन काल तक ही मन निरुद्ध होता है। साधन काल के बाद वह फिर चंचल हो जाता है। और मन को रोको तो मन, मन रहता है। चन्द वक्त के लिए रुक तो जाता है साधन से मगर मन का वजूद नहीं मिटता । और इसको न रोका जाय तो ये रहता ही नहीं। तो मन को अमन बनाने का यही साधन है कि मन को मत रोको । मन के अमन करने का यहो चाहिए । क्योंकि कुछ करने को तो बताते नहीं है। और करने वाला यहां है नहीं । मजा करो फिर क्या है ?
व्यापारे खिद्यतेयस्तु निमेषोन्मेषयोरपि ।
तस्पालस्य धुरीणस्य सुखनान्यस्य कश्चन ।॥
आंख के खोलने और बद करने का जो व्यापार है, तो श्रुति कहती है आंख के खोलने और बंद करने में भी जिसको थकावट मालूम पड़े, ऐसा जो आलस्य घुरीण पुरुष है संसार में वही सुखी है। तो ये लोग आलस्य धुरीण हैं। कुछ नहीं करना धरना, बस थोड़ा सा धान पैदा हो गया । साल के साल नौकर छोड़ देता है। शायद वैशाख में बैठ जाता है। तो बड़े-बड़े बाबुओं को हमने देखा है। नौकर जब सोया रहता है तो उसके पीछे खड़े होते हैं और जगाते हैं-खेदू, बैसाखू ? बोलता ही नहीं है। क्योंकि पा गया हैं न, आलस्य धुरीण पद । तो भगवान ने सोचा, प्रकृति ने सोचा, कि हम दूसरे साधू को यहां भेजेंगे तो ये काम नहीं होगा । तो ऐसे महात्मा को भेजा जाए जो आलस्य धुरीण पद का प्रवक्ता हो । क्योंकि हम कहते हैं। कि मन का निरोध मत करो क्योकि तुम्हारा किया वह होगा नहीं।
तो मन के निरोध में मन अमन नहीं होता, मन बना रहता है। साधन द्वारा मन का जो निरोध किया जाता है उसमें मन का अस्तित्व खतम नहीं होता । साधन काल तक ही मन निरुद्ध होता है। साधन काल के बाद वह फिर चंचल हो जाता है। और मन को रोको तो मन, मन रहता है। चन्द वक्त के लिए रुक तो जाता है साधन से मगर मन का वजूद नहीं मिटता । और इसको न रोका जाय तो ये रहता ही नहीं। तो मन को अमन बनाने का यही साधन है कि मन को मत रोको । मन के अमन करने का यही परम साधन है कि मन को मत रोको । जी हाँ ! अरे देखो न ! अभी तक मन को रोकने का साधन तुमने किया है और रोकने से जो कुछ मिला है इसके साक्षी तुम्ही हो। तो अब मन न रोको । वहां से श्रृंखला चली है कि स्वरूपस्थ होने के लिए ही मन का निरोध किया जाता है।
तो शंका होती है कि क्या मैं स्वरूप में स्थित ही हूँ। निरोध के पहले । हां हूँ तो, मगर स्वरूपस्थ हूँ इसका अज्ञान है । और इसी के लिए मन का निरोध किया जाता है । तो स्वरूप आत्मा में, अपने आप में तो मैं पहले से ही स्थित हूँ। तो इसका प्रमाण क्या है ? कि में पहले से स्थित हूँ ।
'स्वरूपस्थता की अनुभूति मन के अनिरोध में निहित है' । यानी मन न रोकोगे तो मन नहीं रहेगा। और मन के न रहने पर तो प्रत्यक्ष अनुभव करोगे कि में स्वभावतः स्वरूप में स्थित हूँ। मन के निरोध में क्षण मात्र के लिए स्वरूप की झलक तो आती है मगर वह झलक अस्थिर है, चिर नहीं है। साधन काल तक है। सीमित है इसलिए स्वरूपस्थता की अनुभूति मन के अनिरोध में निहित है। क्या प्रमाण है ? यहां पर दो पक्ष हम बतायेंगे । स्वरूपस्थता से मन का अनिरोध होता है और अनिरोध से स्वरूपस्थता की अनु- भूति होती है। फिर देखो । स्वरूपस्थता से स्वरूप में स्थित होने पर, मन का अनिरोध होता है यानी मन को निरोध करने का विकल्प नष्ट हो जाता है। एक, अथवा मनको न रोकने पर स्वरूप- स्थता की अनुभूति होती है। दोनों का अनुभव करायेंगे । एक बार और सुन लो । स्वरूपस्थता से, स्वरूप भगवान आत्मा में स्थित होने पर मन के निरोध का जो विकल्प है उसका अभाव हो जाता है। फिर उसको ये विकल्प नहीं उठता कि मन का निरोध करो और मन को न निरोध करने पर, मन को न रोकने पर स्वरूप- स्थता को अनुभूति होती है क्योंकि मन को न रोकने पर मन अमन हो जाता है।
अब इसका अनुभव करो । निरोध का बोध और निरोध का अनुभव न करायेंगे क्योंकि वो साधन प्रकरण है। अभी यह कथा सुनने आये हो और कथा सुन रहे हो । आनन्द ले रहे हो। कोई पूछेगा-स्वामी जी ! बिना रोके कैसे मन रुकेगा? तो भैय्या ! हम यहां रोकना नहीं बता रहे हैं। हम कहते हैं मल रोको । तो यह आनन्द जो ले रहे हो वह मन के निरोध में कि अनिरोध में ? संमार के तुम्हारे जितने कार्य होते हैं, मन के अनिरोध में ही तो होते हैं। अनुभूति जगत में चल रहे हो भला । अब ये विचार करना है कि मन को न रोकने के लिए भी कुछ करना पड़ता है कि नहीं ? अरे यार, स्वरूपस्थ होता भी तो मन को नहीं रोकते तुम । मगर तुम भगवान आत्मा स्वरूपस्थ न होते तो मन को रोककर के तुम सब काम करते । ये स्वरूपस्पथता का अनुभव करा रहे हैं कि तुम स्वभावतः स्वरूपस्थ हो, जानते भर नहीं हो । और स्वरूपस्थ होने के ही कारण तुमको मन रोकने की जरूरत नहीं पड़ती । अगर तुम भगवान आत्मा स्वरूप में स्थित न होते तो कोई भी कार्य करने के लिए तुमको मन को रोकना पड़ता । भगवान आत्मा की देन है । स्वरूपस्थत्ता ही तो भगवान आत्मा का सतत चिन्तन है। शिव । 'तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च (गीता) । यदि में आत्मा, में स्वरूप भगवान आत्मा स्वरूपस्थ न होता तो किसी भी कार्य के करने के लिए मन के निरोध के लिए कोई न कोई साधन करता में। साधन करना पड़ता। यही स्वरूपस्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
अब कौन सा काम रह गया बाकी, जिसके लिए में मन का निरोध करू । अच्छा, ये स्वरूपस्थता का ज्ञान कराया गया अभी । अब विचार ये करना है कि । तो इसलिए मन के विरोध के लिए कोई साधन यदि करू ? मन को रोकोगे तो मन को मानकर रोकोगे कि जानकर ? मानकर । मन है ऐसा मानकर ही तुम मन को रोकने का प्रयास करते हो । और मन अब रोका नहीं जाता तो 'है' ही रह जाता है। मन को रोक्ते हो तो मन है, ऐसा मानकर । और मन न रोका जाय तो फिर 'है' रह जाता है। मन नहीं रहता। याने अस्तित्व रह जाता है। है अगर न हो अस्तित्व तो मन मानोगे किसको ? कोई न कोई विकल्प का आधार तो होना चाहिए । मन है इसका विकल्प अपने पर करते हो कि गैर पर ? अपने आप पर । अगर और भी जितने कार्य हैं, कोई भी काम करने के लिए, किसी विषय का अनुभव करने के लिए मन की याद हो नहीं आती । मन की जब याद नहीं करते हो तो, मुझ आत्मा के याद करने में मन पैदा होता है या न याद करने में ? मन को याद करना, मन का स्मरण करना, यहां तो मन को पैदा करना है। सबेरे जो हाल में बैठते हो जब, सबके सब, आठ से साढे आठ तक तो मन के निरोध में बैठते हो कि मन के अनिरोध में ? अनिरोध में । मन की स्मृत्ति में बैठते हो या विरमृति में । मन का अनिरोध ही तो अनभ्यास है मन को रोककर जो किया जाय उसका नाम अभ्यास है और मन कोन रोककर किया जाय उसका नाम अनभ्यास है। और अनभ्यास ही भगवान आत्मा का चिन्तन है, जो अचिन्त्य रूप का निरूपण हो रहा है। अब एक प्रश्न होता है कि जब में सर्वथा अपने स्वरूप में स्थित हूँ और स्वरूपस्थ होकर हमारे सारे व्यवहार हो रहे हैं तो जो तुम बेठाते हो आधा घटा हाल में, तो क्या जरूरत है बैठने की। ऐसा प्रश्न करना स्वाभाविक है। और रात दिन सब काम स्वरू- पस्थता में हो रहे हैं तो एक घंटे दो घटे अनभ्यास में बैठने की क्या जरूरत है ? कोई जरूरत नहीं । अगर यह जम जाय तुमको । कोई जरूरत नहीं हैः इसका अनुभव करने के लिए ही जरूरत है ।
अगर ये बात है, अगर तुम बीतराग हो, प्रपंच से अलग हो, आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, कोई पिडा पानी देने वाला नहीं है, मरने के पहले क्रिया कर्म कर सकते हो तो । गरज ये है-
बीतरागभय क्रोधैर्मुनिभिर्वेद पारगैः ।
निविकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोडद्वयः ॥
(गौ. पा. कारिका वैतथ्य प्रकरण ३५)
जो बड़े बड़े बीतराग महात्मा हैं, कल्पना रहित जिनका हृदय है, जो अमन लोग हैं और वैराग्य की मस्ती में रात दिन घूम रहे हैं। संसार जिनकी दृष्टि में है ही नहीं, न जीने में खुशी है न मरने में गमी है, ऐसे लोग चाहे बैठे चाहे न बैठे । मगर भैय्या! तुम लो रात दिन प्रपंच में रहते हो, आज कोई जन्मता है तो कल को मरता है. आज बन रहे हो तो कल बिगड़ रहे हो । ये बवंडर है और वैराग्य है नहीं । या तो गृहस्थ हो रहो या बाबा ही बतो रात दिन तुम रहते हो प्रपंच में, बवंडर आता रहता है तुम लोग के ऊपर । उड़ जावोगे बवंडर में । इसलिए अनभ्यास करना बहु जरूरी है। रात दिन जो सुन रहे हो, उसको कार्यान्वित करो नहीं तो बद्ध ज्ञानी रहोगे । मुक्त ज्ञानी नहीं होगे । इसलिए बड़ी जरूरत है इसकी । और तुम लोगों में, गृहस्थों में ही हम प्रचार करते हैं। क्योंकि गृहस्थ दयनीय होते हैं। कितनी कितनी मुसीबतें गृहस्थों के ऊपर आती हैं। और इतनी मुसीबत झलते हुए भी सत्संग में जाते हैं, जो कुछ बनता है दान पुण्य करते हैं तो हम तो गृहस्थों का कल्याण करते हैं। तुम सबों के लिए ज्यादा जोर है। ये जो अलौकिक ज्ञान है कि तुम सब लोग आनन्द ले रहे हो। तो घंटा दो घटा इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास से ज्ञान की स्थिति परिपाक होती है। गुरु कोई मंत्र बताते हैं तो कह देते हैं, इसका एक लाख जप करना, दस लाख जप करना तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है, अनभ्यास करोगे तो ये स्थिति परिपाक हो जाएगी। फिर एक रस स्थिति हो जायगी । फिर कुछ करने को तो हम बता ही नहीं रहे है। और कहो कि बैठने में कमर दुखता है हम रोगी हैं। हम तो यह बता रहे हैं कुछ न करने की जो अनभ्यास में बैठतें हो, बैठ गये आनन्दा में । जो विरक्त हैं उनके लिए वैराग्य साधन है स्थिति परिपाक करने के लिए और गृहस्थों के लिए अनभ्यास का अभ्यास साधन है।
वैराग्य बोधौपुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौविजानीति विचक्षणत्वम
विमुक्ति सौधाग्रतल धिरोणंताभ्या विनानान्यती रणंसिध्यति ।।१७।।
जैसे कहीं पर पक्षी बैठा हो, एक पंख से कोई चिड़िया नहीं बत्ती, उसी तरह मुमुक्षु रूपी पक्षी के दो पंख है बोध और वैराग्य माने स्वरूपज्ञान और वैराग्य । अब वैराग्य का स्वरूप हम बताते है। सुनो। 'अत्यंत वैराग्यवतः समाधिः'
कहते हैं कि निविकल्प समाधि का लाम किसको होता है ? अत्यंत वैराग्यवान को । अन्यंत वैराग्य का क्या स्वरूप है? क्या अत्यत वैराग्य ही है जो रामजी ने बताया है। यानी मुझ भगवान आत्मा से भिन्न कुछ नहीं । म सब हूँ । वैराग्य का मतलब त्याग ही है न ! वैराग्य के माने त्याग । तो त्याग दो प्रकार का होता है। एक तो विषय के अस्तित्व का और एक प्रपंच के विलास का।
जानिय तबहि जीव जग जागा ।
जब सब विषय विलास विरागा ।।
वैराग्य के दो प्रकार हैं। एक पर और एक अपर । विलास विरागा, नकि विषय विरागा । सन्त महात्माओ के सत्संग से, शास्त्रों के विचार से जो प्रपंच से । आत्मा नित्य है प्रपंच अनित्य है, पुनः पुनः विचार करने से विवेकिनो बुद्धि द्वारा प्रपंच के विलास का त्याग कर देना, चित्त का खिन्न हो जाना ये अपर वैराग्य है। पर जिन जिन विषयों का त्याग किया है, उन उन विषयों का हृदय में अस्तित्व बना है । ये अपर वेराग्य है। इस वैराग्य से गिर जाने का भय रहता है। लोग जब घर छोड़ते है तो भगवान के पास प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलायेगे धन की याचनानकरेंगे पेड़ के नीचे सो जायेगे । ये प्रतिज्ञा करके निकलते हैं। मगर भगवान की माया बड़ी विचित्र है। वो वैराग्य गिर जाता है। आज ही मक्खन निकालो और घी बन लो तो इतनी खुशबू होती है कि घर महन महा जाता है। और उसी मक्खन को दो माह रख लो तो कीड़ पड़ जायेंगे । तो वैराग्य हुआ मक्खन और ज्ञान हुआ घी । तो जब वैराग्य जग तो वैराग्यवान के लिए संत महात्मा संसार में विचरने की आज्ञा नहीं देते । ऐसा न हो कि वैराग्य मंद पड़ जाय । फिर प्रपंच बनाने लगे तो इस विचार से वैराग्यवान को संसार में विचरने की आज्ञा नहीं देते । खुष्ट न्याय से वैराग्य को एकान्त में रहकर पकाना चाहिए और सद् शास्त्र माने वेदान्त शास्त्र का विचार करे और इस खोज में रहे कि आत्म नैष्ठिक सत्त मिले तो उनकी शरण में होकर आत्मा का अनुभव करे । जब तक बोध नहीं तब तक गिरने का डर है। अब ज्ञान का स्वरूप सुनो ।
'जानिय तर्बाह जीव जग जागा,
जब सब विषय विलास विराग़ा ।।
ये अपर वैराग्य हैं। पर वैराग्य कहां है अरण्यकांड में
कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनि गुण त्यागी ।
यहाँ पंच के अस्तित्व का ही त्याग हो गया । जिस संसार को छोडकर मैं निकला था वो हैं ही नहीं तीनकाल में । एक पंख तो ये हो गया। अब ज्ञान का क्या स्वरूप है ? अपने में आत्मा को कुछ न मानकर मैं का मैं ही जानना, ये ज्ञान है। मो मुमुक्षु पक्षी के दो पंख हैं। वैराग्य और बोध । तब तो निर्दिष्ट स्थान में पहुँ- चता है। इसलिए अनम्यास करो जरूर ।
तो अचिन्त्य पद का विवेचन हो रहा है। तो में आत्मा अमनस्क हूँ-
आत्मसत्यानु बोधे न संकल्पयते यदा ।
अमनस्तां तदायाति गात्याभावे तदग्रतम् ।।
सत्य आत्मा के बोध हो जाने पर जब यह मन संकल्प नहीं कर्ता संकल्प रहित होते ही अमन पद को प्राप्त हो जाता है और ग्रहण त्याग से रहित हो जाता है। सत्य भगवान आत्मा का बोध हो जाने पर मन संकल्प और विकल्प से रहित हो जाता है, मन को न रोको तो मन के न रोकने पर फिर मन ही कहां है जो संकल्प और विकल्प करे। रोकने पर तो संकल्प विकल्प है और न रोकने पर यह मन संकल विकल रहित होकर अमनस्क पद जो मैं हूँ। आत्मा, उसको प्राप्त हो जाता है। फिर न ग्रहण रह जाता है नत्याग रह जाता है तो अनभ्यास हम इसलिए समझा रहे हैं। परन्तु इतना ख्याल जरूर रहना चाहिए ।
दूसरा प्रमाण-में स्वरूपस्थ हूँ, स्वरूप में ही स्थित हूँ इसका क्या बात प्रमाण है ? इसका यही प्रमाण है कि विचार के उदय और अनुदय आ में, विकल्पो के उदय और अनुदय में मन के आने और जाने में, मन होत की स्थिरता में और चचलता में जब हर्ष शोक न होय तब में स्व- अ रूपस्थ हूँ। तब समझ लेना कि यही स्वरूपस्थता की अनुभूति है बत क्योकि मन को चंचलता और स्थिरता म, मन के आने और जाने प्र में मन के उदय और अनुक्ष्य में जब ग्लानि और प्रसन्नता, यानी हर्ष और शोक तभी होगा जब पर भाव में रहोगे। और जब स्वरूपस्थ हूँ मैं। जैसे मस्ती में बैठे होऔर कही विशष आवाज आई तो मन चला जाता हैतो मन के चले जाने म क्या तुमको ग्लानि होती है या उसको रोकने का प्रयास करते हो? और मन जब आ जाता है अपने पास ही तब क्या हर्ष होता है? नहीं। यही स्वरूपस्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। य अमनस्क पद समझाया जा रहा है। जब अभ्यास में बैठते हो, अभ्याग करने के लिए तो तुमको देश काल की जरूरत है, कहां बैठें, मगर अनभ्यास का अभ्यास करने के लिए तो बाआर में भी बैठ सकते हो क्योंकि प्रपंच होगा तब न हर्ष शोक होगा ।
एकमेवाद्वितीययद गुर्रोवाक्येन निश्चितम् ।
एतदेकान्तमित्युत्क न मठो न वनान्तरम् ।।
गुरु के वाक्य द्वारा जब ऐसा विश्वास हो गया कि मुझ आत्मा के मिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं तो फिर यही एकान्त है। यही निर्जन है और न मठ एकान्त है न वन एकान्त है। अब अनभ्यास में बैठने पर ये शब्द जैसे (ताली) सुनाई पड़ी तो ये जो (तालो) सुनाई पडी या अक्षर वाला कोई शब्द सुनाई पड़ा । मनोहरलाल ये अक्षर बाला शब्द है । तो सुनाई तो पड़े मगर जो शब्द सुनाई पड़े उसके आकार में मन परिणित न हो। उसके आकार में मन अगर परिणित होता है तो उसका नाम ही ससार है। और सुनाई पड़ने के बावजूद अगर मन परिणित नहीं होता तो में भगवान आत्मा हूं। दोनों बातें बताई जा रही है। फिर सुनो। प्रपंच से हर्ष और शोक होता है तो प्रपंचाकार जब मन होगा तभी हर्ष और शोक होगा और हर्ष शोक न हो यदि तो वो मन नहीं है, में आत्मा हूं।
जब देखो, प्रपंचाकार मन न हो और प्रपंच के आकार में मन परिणित हो जाने पर ही हर्ष शोक होता है। तो प्रपचाकार मन न हो उसके लिए वही डंडा रखो- 'में हूं', शब्द में हू, स्पर्श में हूं, रुप में हू, रस गंध में हूं । "ओमित्येक्षर मिदं सर्वम्" । कुछ ही काल के इस तरह प्रयास से चाहे भैय्या तुम्हारे कान के पास कोई ढोल बजे, उससे तुम्हें ग्लानि न होगी । एक रस स्थिति हो जायगी । हम वही वीज बत्ताएंगे जिसका हमने अनुभव स्वयं किया है और हजारों साखों पर किया है। ये साहित्य नहीं है। ये प्रेक्टिकल है और स्वानुभव है। वो हथियार न फैकना, जरुर रखना वो हथियार। प्रपचाकार नहीं होता तो हथियार अपने पास रखो। मैं हूं कहने की जरुरत नहीं है। और मन बनने लगे प्रपंच, मैं हूं का मारो डंडा अरे मन ही न रहेगा। ये अचिन्त्य के चिन्तन के लिए ही है।
प्राणापानयोर्मध्ये चिदात्मानयुयास्यते ।
मननो मननं यत्य बुद्धेरेकाव बोधनम् ।
जो मन का मन है, बुद्धि की बुद्धि है और प्राण और अपान दोनों के मध्य में जो बैठा है उस चिदात्मा ब्रम्ह की हम उपासना करते हैं। वही हमारा आराध्यदेव है ।
ऊध्वं प्राण युन्नपवत्यपानं प्रत्यगस्यति ।
मध्येवामनभासीनं विश्वे देवा उपासते ।।
जो प्राण को ऊपर फेंकता है और अपान को नीचे फेंकता है प्राण और अपान के बीच जो बैठा है, ब्रम्हादिक जिसकी उपासना करते हैं ।
जो बाहर से सांस लेते हो, जो आक्सीजन है उसका नाम प्राण है। भोतर से जो हवा निकलती है उसका नाम अपान है। जो प्राण और अपान के मध्य में बैठा है, प्राण भीतर गया और जाकर अस्त हो गया । अब जब तक अपान का उदय न हो, वायु जब तक बाहर नहीं निकला, दोनों के बीच में देखो, अब कौन है ? एक पल भर के लिये प्राण को रोककर देखो फिर । कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं । हमेशा रोकने की जरुरत नहीं है। ये तो तुमको अनुभव कराने के लिए बता रहे हैं। बिल्कुल संकल्प रहित अवस्था है। यही सता- तन ब्रम्ह अपना स्वरुप आत्मा है। बिल्कुल कलना रहित अवस्था है । निस्संकल्प । ये महात्मा भुशुद्धि की समाधि है। ये भी भगवान आत्मा के चिन्तन का एक प्रकार है। इसमें प्राण अपान कुछ नहीं रोकना पड़ता । प्राण वायु खट से स्थिर हो जाता है। ये ब्रम्ह पद है। परम पद है। साक्षात् सनातन ब्रम्ह का स्वरुप है। और हाथ से पकड़कर थोड़ी बताया जाता है। स्वयं ही इसका अनुभव करोगे।' अब झपान उदय हुआ । अब जब तक प्राण का उदय न हो, अब जब तक प्राण न आवे, काल जो खाता है वो प्राण को ही खाता है। इस अभ्यास के अभ्यासी को काल भी नहीं खाता । हम तो हमेशा लालायित रहते हैं, तुम्हारे अन्दर क्या भर दें। अब इसकी कदर करना, न करना तुम्हारे ऊपर है। वायु खीचने का नाम पूरक है। जब तक न निकले कुंभक और जहां निकला रेचक ।
संधि में जो ब्रम्ह का ध्यान है, यही सध्या है। इसी पद को जानकर ही मानवता सफल होती है और मानव जीवन की यही सफ- लता है। प्रपच रुत्री व्याज अदा हो गया, मैं ही मैं, मूल रह गया । इसी में जीओ । बस ।
नान्तः प्रज्ञम् …………………….. सविज्ञेयः
अब चार बज रहे हैं, आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है ।
ॐ पूर्ण मदः पूर्ण मिदं, पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण मेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति !!!
षष्ठम् दिवस का प्रवचन
(शनिवार दिनांक १७ नवंबर सन १९७३ समय १० से १२ बजे)
ओमित्येदक्षर ………………..ओकारेव
(संपूर्ण उपनिषद् पाठ)
नान्तः प्रज्ञम् .... स विज्ञेयः
मैं आत्मा न भीतर को जानता हूं, न बाहर को जानता हूं, न मैं प्रज्ञान हूं न अप्रज्ञान हूं। मैं भगवान आत्मा अदृष्ट हूं । अदृष्ट होते हुए अग्राह्य हूं, अग्राह्य होते हुए अव्यवहार्य हूं, अव्यवहार्य होते हुए में आत्मा अलक्षण हूं। और अलक्षण होते हुए में अचिन्त्य हूं। अचिन्त्य का विषय परसों भी हुआ था और कल भी दिन भर चला यहो विषय । जब मैं आत्मा अचिन्त्य हूं। क्योंकि इस मंत्र में भगवती श्रुति ने क्रमशः भगवान आत्मा का विशेषण दिया है । अदृष्टम् में अदृष्ट हूं। किसी करके देखा नहीं जा सकता। मैं अदृष्ट हूं इसके बाद आता है अग्राह्य हूं । व्यवहार में जब नहीं आता तो अलक्षणम् । अलक्षण ह ते हुए और अचिन्त्यम् (आकारु प्रकार ही नहीं है। किसी प्रकार का मुझ आत्मा का लक्षण हो नहीं है तो अचिन्त्य होना स्वाभाविक बात है इसलिए मैं आत्मा अचिन्त्य हूं । तो जब में आत्मा अचिन्त्य हूं तो आत्म चिन्तन का क्या स्वरूप है ? आत्म चिन्तन का क्या लक्षण है जिसके संबंध में कल खूब विवेचन हुआ है और सुन्दर सुन्दर अनुभूतियां आई हैं और कराई गई है। अचिन्त्य होते हुए अव्यपदेश, जिसके लिए किसी किस्म का सकेत न हो । व्यपदेश के माने होते हैं संकेत के । में आत्मा अव्यपदेश हूं माने संकेत रहित हूं । यानि जिसके लिए कोई इशारा है ही नहीं। न तो दृष्टि से कोई संकेत किया जा सकता है, हाथ से कोई सकेत नहीं, मन से कोई संकेत नहीं किया जा सकता, चित्त से जिसके लिए कोई सवेत नहीं है, और न वाणी ही द्वारा कोई संकेत है । वाणी द्वारा यदि मुझ आत्मा के लिए कोई इशारा हो तब तो ये भी कहा जा सकता कि में आत्मा सत् हूँ, चित हूँ, आनन्द हूँ, में आत्मा कूटस्थ हूँ, साक्षी हूँ, नित्य हैं, वाणी द्वारा कहना भी तो एक संकेत है न । वाणी कह ही नहीं सकती जिसको ।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मन सासत ।
आनन्द ब्रह्मणोविद्वान नबिभोति कुतश्चनेति ।
'तैत्तिरीयोपनिषद'
अत्यपदेश में आत्मा क्यों अचिन्त्य हूँ, क्यों कि अव्यपदश हूँ । कुछ कहा ही नहीं जा सकता । जिस तरह । जिस प्रकार में आत्मा सहज हूँ तो जब मैं आत्मा सहज हूं तो मुझ आत्मा को जानना भी सहज है। जो सहज होता है उसको जानना भी सहज होता है। काल्पनिक पदार्थ को जानना सहज नहीं होता, कठिन होता है। मगर जो कल्पनातीत पदार्थ होता है, तो कल्पनार्त त तो सिवाय मुझ आत्मा के विश्व में कोई पदार्थ है नहीं। इसलिए में आत्मा सहज हूँ तो मुझ आत्मा का ज्ञान भी सहज है। जब में आत्मा सहज हूं तो मुझ आत्मा का चितन भी सहज है क्योंकि सहज का ज्ञान सहज, सहज का चिन्तन सहज. सहज की प्राप्ति सहज, सहज का अनुभव सहज । सब सहज ही सहज है। और सहज की समाधि भी सहज है। देखो जितने बेठे हो दोनों समाज में। मैं हूं, अमुक विद्वान, नर, नारी, बालक, युवा, वृद्ध, आस्तिक, नास्तिक, में हू, किसी को सहज हो और किसी को कठिन हो ऐसा तो नहीं है। जो मैं हूं, ये जिस प्रकार एक प्रकांड विद्वान के लिए सहज है उसी तरह एक महान् मर्च के लिए भी सहज है। जिस तरह एक महान आस्तिक के लिए में हूँ जितना सहज है उतना ही ये कट्टर नास्तिक के लिये भी सहज है। तभी तो सार्वभौम है। सार्वभौम उसको कहते हैं जिसका संसार में कोई विरोधी न हो । हरेक सिद्धांत के, हरेक मत के, हरेक मान्यता के जितनी भी चीजें हैं, मैं आत्मा के सिवाय सब का कोई न कोई विरोधी होता है परन्तु में हूं, इसका विरोधी विश्व में कोई नहीं है। और कौन है जो अपने में का विरोधी होगा। भाई । मैं आत्मा सबके अनुकूल हूं । इसका विश्व में कोई विरोधी नहीं। कहीं भी चले जाओ, इस सिद्धांत की अव्याहत गति है। अव्याहत गत्ति उसको कहते हैं कि कहीं भी जाने के लिए पासपोर्ट लेने की जरूरत न पड़े। इसलिए इसकी गति अव्याहत है । कोई भो संसार में इसका विरोधी नहीं ।
आज से पांच छः साल की बात है। हम आँख की जांच कर- वाने गए थे लुधियाना । डाक्टर पाठक हैं। आई स्पेश्लिस्ट है। वो कुछ गीता वगैरह पढ़ते रहते हैं । उनने कहा । स्वामी जी ! आप क्या काम करते हैं मैने कहा निविरोध सिद्धान्त का प्रचारक हूं।
संसार में सबके विरोधी मिलेंगे पर जो में हूं आत्मा, सबके अनुकूल होने के कारण, इसका विरोधी कोई नहीं है। यह निवि- रोध सिद्धान्त है। और निर्विरोध होने के ही कारण में भगवान हूं। जो में नाम से अभिव्यक्त हो रहा है, निविरोध होने के ही नाते में आत्मा भगवान हूं। इसमें तुम्हें लक्षण लगाने की जरूरत नहीं है और वेदान्त की प्रक्रिया समझाने की जरूरत नहीं है । अगर काई मैं का विरोध करता है तो 'मैं' भगवान नहीं, और 'मैं' का कोई विरोध नहीं करता, संसार में एक चींटी से लेकर ब्रम्हा तक फोई विरोधी नहीं है तो डंके की चोट पर में आत्मा भगवान हूँ । इतना कह देना काफी है। अब में आत्मा भगवान हूँ. में भगवान है तो ये लोग झिझकते क्यों हैं ? इस निश्चय में, इस धारणा में, इस सिद्धान्त में, इसकी अनुभूत्ति में लोग झिझकते क्यों हैं-क्योंकि में का मतलब साढ़े तीन हाथ का लगाते हैं, इसलिए झिझकते हैं। शरीर दृष्टि को लेकर झिझकते हैं-में आत्मा सहज हूँ और भगवान भी सहज है ।
'जाहि न चाहिय …………….. सहज सनेह'
अगर भगवान राम सहज न होते तो वाल्मीकि जी ऐसा नहीं कहते ।
'जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम सन सहज सनेह'
जो सहज होता है उसके प्रति प्रेम भी सहज होता है। बनावटी पने का काम ही नहीं है। सहज का ही स्नेह होता है। सहज में ही सहज समाधि होती है और सहज का आनन्द भी सहज होता है। तो मैं हूँ इसका विरोधी कोई नहीं है । सर्वमान्य सिद्धान्त है, इसकी - प्राप्ति भी सहज है । प्राप्ति सहज इसलिए है कि जिसको प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का साधन न करना पड़े, भगवान आत्मा को जानने के लिए किसी प्रकार का, कुछ भी साधन न करना पड़े। साधन तो कठिन के लिए करना पड़ता है परन्तु जो सर्व है, सर्व का अपना आप है, उसको प्राप्त करने के लिए उसे हाँसिल करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर ये कहो कि इसकी सरलता ही कठिनाई है। जैसे राज्य वैभव, ये सब कठिन है, तो लोग इसके लिए साधन करते हैं, इसी तरह सहज स्वरूप भगवान परमात्मा भी कठिन होता तो लोग इसको कठिन न मानते । किसी के पास धन नहीं रहता तो कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, धनवान बनने के लिए । स्त्रीवान बनने के लिए, रूपवान बनने के लिए । ये सब कठिन हैं। मगर इनकी प्राप्ति करने लिए लोग कठिन से कठिन साधन करते हैं। इसी तरह भगवान भी यदि कठिन होता तो ये निविव द है कि लोग इसे कठिन नहीं मानते । ये इतना सहज है। स्वरूप आत्मा इतना सरल है कि इसकी सर- लता ही कठिनाई है। अब में आत्मा सहज का ज्ञान भी सहज है । और उस ज्ञान को जानना भी सरल है ।
देखो-सहज ज्ञान उसे मूर्ख में, विद्वान में, नर में, एक सा हो । जो सत्र में एक कहते ह, जो सब में, पशु में, पक्षी में, नारी में, कीट में, पतंग में, जो सबमे रस हो । जो ज्ञान कभी घटे और बढ़े नहीं, जो ज्ञान कहीं बाहर से आता नहीं उसे सहज ज्ञान कहते है और यह सहज ज्ञान ब्यापक होकर रहता है सबमें । सामान्य होकर और सहज रूप में । किसी शाकाहारी के सामने यानी जो घास फूस खाते है जानवर, उनके सामने तुम मांस रख दो, उसे ज्ञान हो जायगा कि ये मेरा खाद्य नहीं है। किसो मांसाहारी जानवर के सामने घांस रख दो तो कभी न खायगा । ये ज्ञान उसमें भी है। देखो-तो पशु पक्षी में थे जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान व्यापक होकर है। यह ज्ञान उसमें व्यापक होकर है ।
एक बार दिल्ली की बात है। हमारे पास एक इंजिनियर आये नवयुवक । कहने लगे, स्वामी जो ! में कुछ समस्या हल कराने आया हूँ । अच्छा ! में ये पूछता हूं कि क्या ईश्वर है ? मैंने कहा- जी हां । रिश्वतखोर में भी है ? जी हाँ । दूकानदार में भी है जो मिलावट करता है ? जी हां । साधुओं में भी है ? कहना ही क्या। जब पापी के अन्दर ईश्वर है तो पापी को पाप करने से ईश्वर क्यों नहीं रोकता ? ये प्रश्न जरा जटिल है। अगर पापी के अदर भी ईश्वर है, तो पाप करने से उसको क्यों नहीं रोकता, अगर उसके अन्दर व्यापक है? मैंने कहा रोकता तो है मगर वो मानता ही नहीं। कैसे रोकता है ? सुनो- कोई पापी, जैसे चोर है, दुर।चारी है, जो व्यक्ति पाप करने के लिए जब तैयार होता है तो उसको इस बात का ज्ञान होता है कि जो में करने चला हूं, ये अच्छा काम है कि वरा काम है, ये पुण्य है कि पाप है, इसका ज्ञान उसको है कि नहीं? पाप करने वाले को होता है या नहीं ? होता तो है। अब बताओ फिर ये ज्ञान उस पापी का है कि भगवान का है ? और क्या भगवान डंडा लगावे । ये चोरी है, ये बुरा काम है, ये दुराचार है. जैसे अपनी बहू बेटी वैसे दूसरों की बहू बेटी । ये महा पाप है। ग्र हक को ठगना महा पाप है। जो तोला भर सोना तौलने के बजाय अगर दस माशा वो तौल रहा है, क्या इस बात को नहीं जानता भीतर वाला कि में दोरी कर रहा हूं । नकली चीज को ग्राहक को देता है, इस बात का ज्ञान है कि नहीं। तो ये ज्ञान उसका है कि भगवान का ? भोतर से धक्का देता है। खबरदार, इस काम को मत कर । करने वाले की बुद्धि म विवेक रहता है तो रुक जाता है और नही हाता तो अवहेलना करता है। उस आज्ञा का ।
सब में लबालब भरा हुआ है, ठसाठस । मानो तब है, न मानो तब है। हर हालत में है। जो उत्तर दिया हमने उसको खूब स्पष्ट कर लेना हृदय में । जो अच्छा काम करता है, उसका भी ज्ञान रहता है। ये जो भीतर ज्ञान था वो ज्ञान तुम्हारा नहीं है। ये भगवान का ज्ञान है जिसका विवेचन हो रहा है। तो फिर ये जान सहज है कि कठिन । भैय्या, यही सहज का स्वरुप है। य ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं किया जाता क्योंकि भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरुप है हो । 'सहज प्रकाश रूप भगवाना ।' जहां कहीं भगवान राम के लिए आया है, तो सहज ही । 'सहर्जाह चले राम रघुराई ।' 'जंकर सहज स्वरुप सम्हारा ।' क्योंकि भगवान राम सबकी आत्मा हैं और शात्मा होने के नाते सहज हैं। अरण्यकांड में भगवान की स्तुति में लिखा है, तुलसीदास जी ने । हे रघुपते ! मैं सत्य कहता हूं कि आप सारे चराचर की आत्मा हैं। याने सबके में हैं। रामायणी बैठे हों तो देख लें । सुन्दर कांड का है ये श्लोक ।
नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।
भत्रितं प्रयच्छ रघुपुंगवनिर्भरां में कामादिदोष रहितंकुरू मानषं च ॥
तो जो सर्व का मैं हो, जो सर्व का सर्व हो, सर्व में सर्व रुप से होकर रहे वही भगवान है, जो भगवान है, वो सहज है। जो सहब है, निर्विरोध है, जो निविरोध है, सार्वभौम है। सब में लबालब भरा हुआ है। अगर भीतर से ये ज्ञान न हो कि जो तू कर रहा है रो भला है कि बुरा है, नीति है कि अनीति है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो समझना उसके अन्दर भगवान नहीं है। ये नित्तात असभव है। कोई झूठ बोलता है तो भीतर वाला समझता है कि में झूठ बोल रहा हूं। कोई भी शराब पीने के लिए तैयार होता है तो जानता है। कि समाज इसका विरोध करेगा। परिवार इसका विरोध करेगा । ये अच्छी चीज नहीं है, ये ज्ञान शराबी का नहीं है। ये ज्ञान भगवान का है। तो भैय्या जो चौपाई में सहज प्रकाश शब्द आता है, तो सहज प्रकाश से ज्ञान को लेना, वो भगवान का रुप है । भला इसमे प्रत्यक्ष भगवान क्या दिखाया जाय । यह जान न पढ़ने लिखने से मिलता है, न कोई इसको सिखाता है.न किनो साधन से मिलता है तभी तो सहज है ।
ये जो सहज ज्ञान है, यही तो में हूं। अब यहां पर एक शका बारीक आ गई । स्वामी जी ! जो पुण्य पाप का कर्ता है, वो क्या मैं नहीं, अगर में आत्मा हूं सहज ज्ञानस्वरुप हूं तो सहज ज्ञानस्वरूप में आत्मा से पुण्यपाप करने वाला भिन्न है? जी हां भिन्न है। क्योकि अपने आपको कुछ मानकर ही पुण्य पाप करता है तो फट से में से अलग हुआ ।
सहज ज्ञान स्वरुप में आत्मा हूं, पुण्य पाप जो करना है तो पुण्य पाप करने वाला सहज ज्ञान स्वरुप आत्मा से क्या अलग है ? जी हा अलग है। कैसे ? वो कुछ मानकर ही तो पुण्य पाप करता है। और जहा अपने को माना तो भगवान से फट से अलग हो गया, भिन्न हो गया और भिन्न होने वाले से ही भगवान भीतर से कहता है कि जो ये कर रहा है, य पुण्य है और ये पाप है। धन्य है इस अध्यात्म को कि विश्व में भगवान का साक्षात् दर्शन करा देने वाला यदि कोई सिद्धांत है तो वेदात ही है। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और देखो यदि अपने आपको कुछ न माना तो फिर वही भगवान है और उस भगवान से न पुण्य होगा रुपाप । उस भगवान के देश में न पुण्य है और न पाप है । प्रपच ही नहीं तीनकाल में । तो भैय्या ! आज संसार के जितने भी क्षत्र है. क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या राजनैतिक, इस अध्यात्म चेतना से शून्य हो रहे हैं। और अध्यात्म चेतना से शून्य होने के हो कारण हरेक क्षेत्र में अनाचार हो रहे हैं, तो जरुरत आज के समार को इस चीज की है। आज का संसार, आज का युग, आज का जमाना, हाथ फैलाकर तुमसे अध्यात्म ज्ञान की याचना कर रहा है। किसी का हृदय कानून से नहीं बदला जा सकता । इस बहिरंग कानून से, वाह्य जगत के कानून से अंतर्जगत का जो हृदय है उसका परिवर्तन नहीं हो सकता । अंतर्जगत का कानून यही है जो सुन रहे हो । और यह अंतर्जगत का कानून सब पर लागू होता है.। कुछ लोग हमें कभी कभी कहते हैं, पढ़े लिखे विद्वान- स्वामीजी ! आप का जो भाषण है, निरुपण है, प्रवचन है, इसका तो ब्राडकास्ट होना चाहिए । में कहता हूं- नाम तो हमें चाहिए नहीं और न हमको कीति फैलानी है दुनियां में । पेंडाल भर के लिए नहीं हो रहा है ये ब्राडकास्ट । देखो मंगलाचरण में सुनते हो- अनन्त नाम-रुपों में अभिव्यवत्त, अहम्त्वेन प्रस्फुरित, सकल चराचर, तो यहीं तक के लिए थोड़े है । ये आवाज तो तीन लोक तक जा रही है। ब्रम्हलोक तक जा रही है।
समझो विषय । सहज ज्ञान । सहज ज्ञान ये है जिसकी अनुभूति अभी कराई गई । सब में बिल्कुल यह ज्ञान किसी से मिला नहीं। इस ज्ञान को किसी ने पढ़ाया नहीं । इस ज्ञान को किसी ने सिखाया नहीं । ये ज्ञान सब में बिना प्रयास के ओतप्रोत है । और यह मैं आत्मा हूं । ये जो सहज ज्ञान है, वह मुझ आत्मा का सहज स्वरुप हैं और ये जो सहज ज्ञान है, यही तुलसी का राम है, सूर का श्याम है, गोपियों का कृष्ण है, मीरा का गिरधर है, ईसाइयों का ईसा है। आस्तिकों का 'है' है और नास्तिकों का 'नहीं' है। यह सहज ज्ञान है। बिल्कुल ओतप्रोत । लबालब भरा हुआ है। मगर अव्यपदेश, जिसके लिए कोई संकेत नहीं । य सहज ज्ञान के लिए क्या संकेत है-कोई संकेत नहीं, कोई इशारा ही नहीं । और इस सहज ज्ञान का ज्ञान महात्माजन कराते हैं। जो सहज ज्ञान स्वभावतः सिद्ध है उसको गुरुजन लखाते हैं। जैसे तुम लख रहे हो और हम लखा रहे हैं। और इसी अनुभूति को सहजानुभूति भी कहते हैं। इसका आनन्द भी सहजानन्द है । परन्तु देखो भैय्या-एक आनन्द तो ऐसा होता है कि जिसमें मन विभोर हो जाता है। मन और इन्द्रियां सबके सब विभोर हो जाती हैं। और एक आनन्द ऐसा होता है कि मन भग- वान हो जाता है। मन विभोर हो जाता है। मगर मन विभोर हो जाने के बावजूद मरता नहीं । मन मरता नहीं, मन बना रहता है। जिसमें क्षणिक आनन्द कहो, नश्वर विषयानन्द । माने समाधि तक का आनन्द भी विषयानन्द है न भला । समाधि भी विषयानन्द ही है। वो चाहे घंटे भर की समाधि हो चाहे एक कल्प की हो । क्यों कि समाधि तो कभी न कभी टूटेगी । और समाधि का आनन्द जो है वह भी विषयानन्द है । मन मरता नहीं, मन कायम रहता है। मगर जो सहजानन्द है, जो सामान्य आनन्द है उसमें तो मन रहता ही नहीं, मन में हो जाता है। मन सहज हो जाता है। मन का बजूद हो खतम हो जाता है। क्षणिक आनन्द में विषयानन्द में तो लोंगटे खड़े हो जाते हैं। आ-हा-हा। मन के विभोर होने की ये नाराज है। मगर जो महजानन्द है उसमें न आ-हा-हा है न ओ- हो-हो। शान्त । इसमें शान्ति का अनुभव होता है। अरे मन हो नहीं रहता तो विभोर कौन होगा । इसलिए एकाएक इस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि इसमें रसास्वाद है नहीं । शून्यता की प्रतीति होती है। जिस तरह किसी व्यक्ति को रात्रि के अंधकार में, निर्जन प्रदेश म उसको वैताल का भ्रम होता है, उसी तरह भग- बान आत्मा के अज्ञान के कारण अज्ञानी को, यद्यपि सब कुछ है, जून्य नहीं हैं, पूर्ण है परन्तु वह पूर्णता में शून्यता का अनुभव करता है। यही सहजावस्था है। ये ही सहज पद है और यहो राम, कृष्ण, शिव, अपना आप है, स्व स्वरूप भगवान आत्मा में हूं इसमें कोई संकेत नहीं है और संकेत रहित होने के कारण अव्यपदेश है। इशारा कुछ नहीं है इसके लिए ।
महाराज ! तुम तो ज्ञानी पुरुष हो, मैं तो अज्ञानी हूँ, ये कह कैसे रहे हो तुम ! अरे, तुझे ज्ञान का भी ज्ञान है, अज्ञान का भी ज्ञान है जिस ज्ञान से ज्ञान अज्ञान दोनों को जान रहा है वो भगवान आत्मा जानी और अज्ञानी कैसे ? सहज ज्ञान के अनुभव में ज्ञान और अज्ञान दोनों का अत्यन्ता भाव है। देखो-
हर्ष विवाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धरम अहमिति अभिमाना ॥
तो भैय्या इस सहजानन्द में, इस सहजानुभूति में गोस्वामीजी ने कहा है-
शोक मोह भय हरष दिवस निशि, देश काल जहें नाहीं ।
तुलसिदास अस दशाहीन संशय निर्मूल न जाहीं ॥
रघुपति भगति करत कठिनई ।।
यहाँ पर ये प्रपंच है ही नहीं । बिल्कुल अविचल, अविरल, अटल, अचल, ऐसा है ये पद, इसलिए में आत्मा सहज हूँ । मुझ आत्मा का अनुभव सहज है । सहज ज्ञान स्वरूप का जो अनुभव किया है उसके लिए कुछ किया था या कभी कुछ करके अनुभव किये हो ? नहीं। ये बात । हमें तो अनुभव कराने में कोई मेहनत नहीं पड़ती । अनुभव करने वाले को भले होय । हमें कोई परिश्रम नहीं । इसमें क्या मेहनत है। इस पर अगर कोई कलई हो, कोई बनावटी पना हो तो फिर इसको देखने और दिखाने में मेहनत हो। अरे जैसा है वैसा ही लखा दिया ।
हां जी ! सहजानन्द, सहजावस्था, सहज समाधि । सहजानुभूति की अनुभूत्ति कराई गई । अब सहज समाधि का अनुभव करो ।
जो समाधि बिना लगाये लगी रहे, जो समाधि लगानी न पड़े, जिसके लिए देश काल की अपेक्षा न हो, जो स्वाभाविक लगी रहे, बिना प्रयास ही, इस समाधि को सहज समाधि कहते हैं ।
सहज समाधि चित्त की नहीं है, सहज समाधि बुद्धि की नहीं है, सहज समाधि मन की नहीं है। सहज समाधि तो मुझ आत्मा की है। सम माने बराबर हो जाय धी माने बुद्धि जिस अवस्था में उसका नाम ही सहज है। जब में हूँ इसकी अनुभूति की तो बुद्धि भी सम हो जाती है। कल तो दिन भर यही विषय चला है। जो कुछ भो तुम व्यवहार करते हो, सहजावस्था में करते हो कि बना- वटी में ? सहजावस्था में । जब सहज ज्ञानस्वरूप में आत्मा हूँ तो किसी भी व्यवहार के पालन करने में मैं आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप रहता हूं कि नहीं ? रहता हूं। तो व्यवहार हो रहा है ? व्यवहार का होनापना बनावटी पने में सिद्ध है या सहजावस्था में सिद्ध है ? बनावटी पने में । मानना बनावटीपना है और न मानना सहजपना है वो त मानने में कुछ नहीं और मानने में व्यवहार हो रहा है। मान कैसे हो अपने आपको तो व्यवहार होना सिद्ध होता है। और मान- कर के ही व्यक्ति व्यवहार में संलग्न होता है। और व्यवहार हो जाने के बाद उसका अपने आपको कर्ता मानता है, मगर व्यवहार के व्यवहार काल में कर्तापन का मान नहीं रहता। वही तो सहजावस्था है, वही सहज समाधि है। घर से जब चलो-कहां जा रहे हो दाऊ ? कथा हो रही है-महामाया मंदिर में, वहां जा रहे हैं। बैठते तक तुमने माना कि में श्रोता हूँ । यह व्यवहार पना है। मगर कथा के श्रवणकाल में श्रोता, श्रवण और शब्द ये तीनों का अभाव हो गया । ये सहजपना है। यह बताया नहीं, पकड़ाया जा रहा है। ये सहजपना है। अब कथा बंद भई, तब इसके बाद श्रवण की जो मान्यता थी उसकी स्मृति फिर आ गई कि इतनी देर सुना। वही जी जी के मरना । एक ढक्कन तो पहले वाला और एक ढक्कन बाद वाला, दोनों ढक्कनों के बीच ये सहजपद छुपा है। भला कौन जाने इसको । इसलिए ये कृपा साध्य है । साधन का विषय नहीं है। एक मान्यता रूपी ढक्कन पहले का, इतनी देर मने सुना । ये व्यवहार है तो ये दोनों ढक्कन है। दोनों ढक्कनों के बीच में ये सहजपद छुआ है ।। इसलिए ढक्कन को उभारना सन्त शरण की देन है। चाहे लिखो, पढ़ो, चाहे योग करो, समाधि लगाओ, वैराग लो । सन्त शरण से ही ये पद सुलभ होता है । फिर शंका हो गई। अब यहां होती है शंका-जब अनुभव कर लिया, संत शरण से ये सहज- पद की अनुभूति हुई तो क्या मान्यता नहीं रहती ? नहीं । मानना ऐसा ही रहेगा । परन्तु मान्यता में जो आस्था है, सत्यता है वह नहीं रहेगी । तो वह जो बीच वाली अवस्था है, ढक्कन वाली वह रह जाती है। वह तो रहती है। बाकी दोनो ऊपर नीचे के ढक्कन हैं उनके प्रति आस्था नहीं रहती ।
जासु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ।।
ये प्रभु प्रसाद कोउ पाव ।
मृग तृष्णा का जल सबको दिखता है, मगर मनुष्य जो है उसमें पीने को नहीं जाता क्योंकि जानता है कि है । दरअसल यहाँ पानी नहीं है बूंद भर भी। मृगजल में आस्था नहीं होती क्योंकि उसको सूर्य सूर्य का करिश्मा मगर उसको उस का ज्ञान है। और जानवर को माने हरिण को इसमें आस्था होती है और उसको सत्य मानकर वो पीने के लिए दौड़ता है उसी तरह से जो जगत प्रपच है, व्यवहार है, मृगजल है, भगवान सहज ज्ञान स्वरुप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश आत्मा का ये करिश्मा है, ये चमत्कार है कि प्रपंच व्यवहार तीन काल में न होते हुए भी सत्य सा भासता है। तो इसमें बोधवान की आस्था नहीं रहती। बाकी बोलता है, चालता है। जैसे सर्राफ की दुकान में जब आभूषण खरीदने जाते हो तो सोना हो खरीदा जाता है और सोना ही बेचा जाता है। आभूषण न खरीदा जाता है, न आभूषण बेचा जाता है। सर्राफ की दृष्टि स्वर्णांकार होती है ।
मगर वो कहेगा तो, कहेगा कि भैय्या-आलमारी से हार निकाल दो । ये न कहेगा सोना निकाल दो । कान की बाली तो निकाल दो, झूमका निकाल दो । देखने के लिए बोलचाल में जिस आभूषण का जो नाम है, कहो कहेगा, मगर आस्था आभूषण में न रहेगी। उसकी आस्था सोने में होती है। इसी प्रकार आत्मा का अनुभव हो जाने पर प्रपंच में, कल्पित पदार्थ में आस्था नहीं होती लेकिन बोल में, चाल में, व्यवहार ऐसा ही रहता है जैसा पहले था। दृष्टि बदल जाती है। वो हमेशा ही सहज पद पर आसीन रहता है। कभी उसको भ्रांति नहीं होती । यही ज्ञान का फल है। यही ज्ञान की महिमा है। तो अज्ञानी को जब विकार आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सुर, तब वह अंधा हो जाता है। कामान्ध, मदान्ध, फिर उसको अपने पराये का विवेक नहीं रहता । परन्तु स्वरुप ज्ञानी ये जानता है कि ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है। जरुरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल करता है, जरुरत न पड़ी तो त्रुटकी बजाकर भगा देता है । बोधवान को बोधवान ही जान सकता है। क्योंकि एक ही व्यवहार होते हैं तो क्या पहिचान करेगा कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है। जो पूर्ण रुप से सहज पद में स्थित होता है उसके सब गुलाम होते हैं। विकार गुलाम हो जाते हैं, मन गुलाम हो जाता है। सब पर उसका आधिपत्य हो जाता है। जीव सवका गुलाम होता है। मगर भगवान किसी का गुलाम नहीं होता । तो तुमको भगवान का ज्ञान कराया जा रहा है। सिर्फ मान्यता ही तो हटाई जा रही है। ऊपर नीचे का ढक्कन उघारा जा रहा है। बीच की जो चीज है। वही लखाई जा रही है क्योंकि में आत्मा सहज ज्ञान स्वरुप अव्य- पदेश हूं यानी मुझ आत्मा के लिए किसी प्रकार का संकेत है ही नहीं कि मैं ऐसा हूं। मैं ऐसा था । ज्ञान प्राप्त किया, इस समय ये हो गया। कुछ नहीं । जैसा में पहले था, जहां में पहले था, वही वैसा ही में अब हूं, वैसा ही आगे रहूंगा। क्योकि में आत्मा सहज हूँ तो। नान्तः प्रज्ञम्... प्रत्ययसारम् उपनिषद् की भाषा में विश्वनीय पदार्थ को प्रत्ययसार कहते है। प्रत्ययसारम् । देखो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं- एक विश्वसनीय एक आदरणीय । जो विश्वास करने योग्य हो, जो विश्वास पात्र हो उसको विश्वसनीय कहते हैं और विश्वास पात्र नहीं है, आदर का पात्र है, उसको आदरणीय कहते हैं। तो सारा संसार आदरणीय है। तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी पत्नी विश्वसनीय नहीं है, आदरणीय है। पुत्र पर विश्वास करना उचित • नहीं है क्योंकि जीने की गारन्टी किसी की नहीं है। धन पर अगर विश्वास करो कि इसी तरह लखपती, करोड़पती हमेशा रहेंगे तो धन भी विश्वसनीय नहीं है, आदरणीय है। उपेक्षा का पाँत्र नहीं है। आदर का पात्र वह है मगर विश्वास पात्र नहीं है। धन का - दुरुपयोग करना । जहां एक रुपये की जरुरत हो वहां दस रुपये खर्च करना । जहां खर्च करना चाहिए वहां वैसा खर्च करो । मगर ऐसा विश्वास न करो कि ये संपत्ति हमारे पास रहेगी। इसलिये महात्मा - गण लक्ष्मी को वेश्या कहते हैं क्योंकि वेश्या एक की नहीं होतो । और वेश्या की दृष्टि में जात पात का परहेज ही नहीं होता । आज लक्ष्मी विद्वान ब्राम्हण के पास है कल किसी नीच कुल में चली जाती है तो उस पर विश्वास करना ये बेवकूफी नहीं तो बुद्धिमानी है? इमलिए जो विरवत सन्तमहात्मा है वो ठोकर मारते हैं, उपेक्षा करते हैं। तो संसार आदरणीय है विश्वसनीय नहीं है। अगर कहो शरीर विश्वसनीय है, विश्वासपात्र है। आज इसको खिलाओ, पहिनाओ। मगर पता नहीं किस वक्त ये भी शांत हो जाय । आदर करो । मगर विश्वास न करो, ऐसा ही बना रहेगा । पता नहीं कब धोखा दे जाय । देखते देखते आंख बंद हो जाय इसलिए इन्द्रिया भी विश्व- सनीय नहीं है। मन पर विश्वास मत करो। कभी बुरे में जाता है, कभी भले में जाता है, कभी निन्दा करता है, कभी स्तुति करता है। इसलिए मन भी विश्वसनीय नहीं आदरणीय है। चित्त पर विश्वास मत करो, बुद्धि पर विश्वास न करो । सांस अंदर से निकल कर बाहर जाता है, और अब आता है भीतर कि नहीं आता, इसका विश्वास नहीं । आदरणीय है, मगर विश्वसनीय नहीं है। उपेक्षा के पात्र नहीं है । प्राण को उपेक्षा क्या है ? करेन्ट पकड़ लेना, मिट्टी का तेल डालकर जल जाना, हत्या कर लेना । तो उपेक्षा मत करो आदर करो, मगर विश्वास मत करो । तो गरज ये. है शरीर प्रपंच धोखेबाज हैं । सबमें धोखा है, विश्वास मत करो। तो प्रश्न होता है। विश्वसनीय क्या है ? तो विश्वसनीय तो सिवाय में आत्मा के कुछ नहीं । विश्वास करना है तो अपने आप पर करो। में आत्मा ही विश्वास पात्र हूं । देखो, जाग्रत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में किसी काल में ऐसा टाईम आता है कि मैं आत्मा न रहूं । नहीं आता। यानी अपने अभाव का अनुभव कभी करता है ? नहीं। जो हमेशा रहे, घटे नहीं, बढ़े नहीं, बंधे नहीं छूटे नहीं। जो अजन्मा होगा उनके लिए बंध कहां और मोक्ष कहां । बंध मोक्ष तो जीव देश का कानून है । मगर मुझ आत्म देश में बंध और मोक्ष का विकल्प नहीं है। में ही विश्वास पात्र हूं। अपने आप पर विश्वास करो । और जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं होता उसको भगवान पर भी विश्वास नहीं होता । आत्म विश्वास ही भगवान पर विश्वास है। और आत्मनिष्ठा ही भगवान निष्ठा है और वही निर्भयपद है और जिसको न आत्म विश्वास है और न भगवान पर विश्वास है उसकी जिन्दगी अन्यथा सिद्धी है। अन्यथा सिद्धी उसको कहते हैं जैसे कुत्ते की पूछ। कुत्ते की पूंछ जो है वो न तो मूलद्वार ढंक सके नं मच्छड़ मक्खो भगा सके । तो जिसको भगवान पर विश्वास नहीं उसकी अन्यथा सिद्धी है कुत्ते की पूंछ जैसे । जिसको अपने पर विश्वास नहीं और भगवान पर, दोनों विश्वास नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीना ही मरना है। वो भले अपनी दृष्टि में समझे कि मैं जिन्दा हूँ, लेकिन मुर्दा है।
सारा संसार आदरणीय है और में विश्वसनीय हूँ ।
समय २ बजे से ४ बजे तक
आत्म जिज्ञासुओ !
नान्तः प्रज्ञम् न बहिः प्रज्ञस् …………………… स विज्ञेयः
उस समय के प्रसंग में प्रत्ययसार का विवेचन हो रहा था और अभी भी वही है। प्रत्ययसार कहते हैं विश्वास पात्र को । जो - पदार्थ विश्वसनीय होता है विश्वास करने योग्य । जिसमें कोई धोखा - नहीं और जो मानने योग्य नहीं जो पदार्थ जानने योग्य होता है, उसमें धोखा नहीं होता और वही विश्वास पात्र कहलाता है। बाकी देहादिक प्रपंच माने जाते हैं। सारा प्रपंच माना जाता है जाना नहीं जाता ।
प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा ।
आद्यन्तवदसद् ज्ञात्वा निःसंगोविचरेदिह ॥
श्री मद्भाग० ११
प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, निगम प्रमाण अनुभव प्रमाण. चार प्रमाणों से जो सिद्ध किया जाता है, चारों प्रमाणों से जो प्रमाणित होता है वही पदार्थ सत्य है और वही पदार्थ विश्वसनीय है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं ? जैसा दिखाई दे, जैसा देखने और सुनने में आवे, उसी प्रकार अपने मूल भाग में भी मिले । वैसे ती रज्जू में सर्प भी प्रत्यक्ष है। अंधेरे में जो सर्प दिखाई देता है, रज्जू में, अरे प्रत्यक्ष ही तो है । प्रत्यक्ष न हो तो भयकपन न लगे। है तो प्रत्यक्ष वो भी, परन्तु प्रकाश में नहीं दिखता, प्रकाश में नहीं रहता । प्रकाश होने पर इस सर्प का अभाव हो जाता है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का होता है । एक बूढ़ प्रत्यक्ष एक अदृढ़ प्रत्यक्ष । तो रज्जू में जो सर्प दिखाई देता है वो अदृढ़ है माने अघरे ही तक है और अधकार के नाश में तो सर्व का भी नाश हो जाता है। वो प्रत्यक्ष तो है पर दृढ़ नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण उसको ही कहते हैं कि जैसा वो देखने और सुनने में आवे तो मूल में भी वैसे ही रहे उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । में आत्मा प्रत्यक्ष हूँ और किसी से अप्रत्यक्ष नहीं हूँ। सबको प्रत्यक्ष हूँ सबमें प्रत्यक्ष हूँ। जो पदार्थ विश्वसनीय होता है, जोखा रहित होता है, विश्वास करने योग्य होता है, ये भी निविवाद होता है कि वह अनेक न होकर सबमें एक होता है। इसका क्या प्रमाण है कि में सर्व में एक हूँ। अनेक में में एक हूँ इसका क्या प्रमाण है ? देखो-यदि अनेक में में अनेक होऊ । में आत्मा का जो जाननपना है, यहां पर जादा हो (स्वामी जी अपने तरफ सकेत कर रहे है) और शरीर में कम हो, किसों में ज्यादा हो किसी में कम हो तो में एक न होकर अनेक होऊ । जितना और जैसा और जिस प्रकार में यहाँ जानता हूँ, इस देश में रहकर, उतना ही, वैसा हो, उसी प्रकार से सबमें रहकर जानता हूँ । जाननेपने में यदि न्यूनाधिक हो अगर कम ज्यादापना हो तब तो ये कहा जा सकता है कि हां में एक नहीं अनेक हूँ। स्वामी जो ! यहाँ पर एक शंका होती है । तो फिर में जब सबने एक हूँ तो फिर तुम ब्रम्ह विवेचन कर रहे हो उसी प्रकार में भी क्यों न करूं, यदि सबमें एक हूँ तो । ब्रम्ह तत्व का विवेचन करना, विश्लेषण करना ये में का काम नहीं है। ये बुद्धि का विषय है ये - पांडित्य है। इन्हीं बातों को लेकर लोगों को इस प्रकार की शंका - होना स्वाभाविक है। न्यूनाधिकता दिखाई देती है । जो में गद्दी पर बैठा हुआ शेरीर है, इसी प्रकार में क्यों न निरूपण करूं फिर । तो ये में का काम नहीं है, ये बुद्धि का विषय है। देखो जैसे महा- सागर भरा है। कितना जल है, कितनी गहराई है ये पता नहीं । अब जिसके पास जितना छोटा बड़ा पात्र हो, समुद्र से भरकर ले आवे । समुद्र तो एक ही है। उसी प्रकार में आत्मा ज्ञान सागर हूँ। "पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि, प्रगट परावर नाथ" 'ज्ञान अखंड एक सीतावर' । लबालब हूँ । सब प्रकार से पूर्ण हू । किसी चीज की मुझ आत्मा में कमी नहीं है। पूर्ण ज्ञान सागर में आत्मा भरा हुआ हूं। अब जिसके पास बुद्धि रूपी पात्र जितना छोटा बड़ा हो, निकालो, भरो । मैं आत्मा तो सबमें ज्ञान पुज एक सा हूं। किसी की बुद्धि छोटी होती है, किसी को बुद्धि बडी । उमको उत्तना ही ज्ञान रूपी जल मिलेगा, जितनी वो होगी उतना ही ज्ञान मिलेगा । तो ये बुद्धि का काम है। इसमें हम प्रारब्ध नहीं मानते । करम में यही लिखा था। ये सत्र बात शंख ढपोरी हैं। तुमने कोशिश कब किया । आत्म ज्ञान सागर भरा हुआ है। तो तुमने कोशिश किया? कि हमारे पास. ज्ञान आ जाय । सव फालतू बात है। करम क्या करेगा । हम प्रारख्धवादी नहीं पुरषार्थ वादी है। ये बात भारत में है. बाहर नहीं है। प्रारब्ध क्या है, सपने में भी इसका नाम नहीं है। और सब तरक्की कर रहे है। कोई काम गड़बड़ हो जाता है तो अपना दोष देते हैं कि यार हमसे गलती हो गई । मगर भगवान ने बिगाड़ा, या प्रारब्ध में यही लिखा है, ये बात विदेश में न सुनोगे । इसलिए देखो कितनी तरक्की कर रहे हैं। ये हमारे ही देश में है। बीमारी। और बिना तत्व बोध के ये बोमारी जाती नहीं ।
'सो परत्न दुख पावई…………………
कोई काम बिगड़ गया तो क्या करें भैय्या-हमारे करम में ऐसा लिखा था। भगवान की ऐसी ही मर्जी है। और काम बन जाय तो अपनी हो मर्जी है। योगवाशिष्ठ महारामायण म ३२ हजार श्लोक है। सन् १९३९ में गुरु पूर्णिमा हुई थी तो हम गए थे डोंग- रगाँव । चार महीने योग वाशिष्ठ की कथा हुई थी । ३२० हजार श्लोक हैं। सब पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। जो हमारा किया हुआ पुरु- षार्थ है वो तीन नाम से कहा जाता है-संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध ।
मैं आत्मा ज्ञान सागर हूं, ज्ञान पुंज हूं। अखंड ज्ञान स्वरूप हूं। मुझ आत्मा का ज्ञान अगर खंडित हो जाय । खंडित उसको कहते हैं-देखो-देखते-देखते आख खंडित हो जाती हैं, चलते चलते पैर का थक जाना, ये पैर का खंडित होना है, हाथ थक जाना । सोचते सोचते दिमाग थक जाता है । चिन्तन करते करते चित्त खंडित हो जाता है, परन्तु वाहरे भगवान आत्मा, इतने दिन हो गए जानते जानते मगर मुझको जानने में थकावट नहीं आई। जानते जानते बहुत दिन हो गया भैय्या, अव थोड़ा आराम कर लेने दो, ऐसा कभी नहीं हुआ । इसलिए ये भगवान आत्मा का जो ज्ञान है वो अखंड ज्ञान कहा गया है। और कब से जान रहा हू ? अरे जब से मैं हूं। कब तक जानता रहूंगा ? जब तक रहूंगा। कब तक रहेगा? ये पता नहीं । कब से हूं ? ये पता नहीं । इसलिए अखंड ज्ञान सागर हूं। इसमें अगर कोई कमी बेसी दिखाई पड़े कि यहां पर में अखंड ज्ञान स्वरुप हूं, उस शरीर में खंड ज्ञान स्वरुप हूं, इसमें कम जास्ती दिखाई दे तब तो माना जाय कि में एक नहीं अनेक हूँ। कि तुम तो ज्यादा विद्वान हो, हम तो कुछ नहीं पढ़े । नहीं, ये बात नहीं है । विद्वता और मूर्खता बुद्धि का धर्म है न कि में आत्मा का । यहां तो मैं का ज्ञान कराया जा रहा है न कि बुद्धि का, न चित्तका, न प्रपंच का या इन्द्रियों का । इसलिए तुलसीदासजी ने कहा- 'ज्ञ न अखड एक' । जो ज्ञान अखंड एक है, सोई सीतावर । ज्ञानअखड एक, सीतावर । अब सीतावर का क्या मतलब लगावोगे ? वर माने स्वामी । सोई सीतावर है। अब सीता किसको कहोगे ? मैं आत्मा अखंड ज्ञान स्वरुप हूं तो मैं तो हुआ राम और मुझ आत्मा पर जितनी मान्यतायें हैं सब सीता है।
जो जिसका आधार होता है, वही उसका पति होता है, वही उसका रक्षक होता है, वही उसका प्रभु होता है, जो मर्जी आए कह लो। तो तृण से सारा चराचर हैं उनका जो मूल कारण, सारे प्रपंच का जो आधार, पति, स्वामी में आत्मा हूं क्योंकि सबकी सिद्धी करता हूं। इसलिए मैं क्या हूं ? ज्ञान अखड एक । मुझ आत्मा का ज्ञान खडित नहीं होता कभी जानने से मैं आत्मा थकता नहीं । जाग्रत अवस्था के प्रपंच को मैं जानता हूं और देखो-जहां पर स्तुति होती है, जहां पर उपदेश होता है वहाँ पर तू शब्द का प्रयोग किया जाता है और जहां पर साक्षात निरुपण होता है, फिर तू कहने की जरुरत नहीं है। अरे भाई जो 'मे' यहां से विवेचन कररहा हु, वहीं 'में' हर शरीर से सुन रहा हूं तो दूसरा कहां से आ गया । तो भैय्या अखंड ज्ञान का यही स्वरुप है। अनुभूति है कि जो मुझ आत्मा का जानना पना है, यह कभी खंडित नहीं होता, क्यों नहीं होता ?
आज दिन तक मुझ आत्मा को जानने से थकावट नहीं लगी । थकावट लगे तो आलस भी लगे । तो जानने से थकावट नहीं लगती तो आलस भी नहीं लगती मुझ आत्मा को । अरे जो में अखन्ड ज्ञान स्वरुप आत्मा हूं 'एक' । अनेक नहीं एक । पशुओं में भी। जिस तरह मैं यहां जानता हूं, उसी तरह पशु पक्षी घोड़े गदहे, वहां भी में जान स्वरुप हूं । अब रही बात बुद्धि की, तुम अपने घर में लगाते रहो । अब पशुओं में बुद्धि नहीं होती विचार करने की । अरे मच्छड़ एक जन्तु है छोटा सा । और रायपुर में तो साम्राज्य है उनका । देखा कितना ज्ञान है उसमें । नाक में नहीं बैठता, मुंह में नहीं बैठता । सवसे पहले फोन करता है कान में । उसको पता रहता है कि यही कान है। कान में ही वीणा बजाता है । जो सो रहा है, इसका कान यहीं पर है। कितनी बुद्धि है । खटमल कितना छोटा जन्तु है। ऊपर से गिरता है ये ।
रही बात बुद्धि की और इन्द्रियों की । ये तो प्रपंच है। किसी की बुद्धि छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो में जो आत्मा हूं, अखंड ज्ञान स्वरुप हूं और सबमें एक हूं। यहो मुझ आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण है । अब भला इससे प्रत्यक्ष और क्या होगा । वाह कान के सुनने को में सुनता हूं । आख वे देखने को देखता हूं आआंख नहीं देखती उसको भी मैं जानता हू मन स्थिर है उसको मैं जानता हूं, मन कहां चला गया उसको में जानता हूं । मानस प्रेमियो ! रामायण के अयोध्या काण्ड से- "सबके उर अंतर बसहु, जानहुभाव कुभाव" । अनेक होकर नहीं एक होकर । सबके उर अतर बसहु, जानहु भाव कुभाव । हरेक में भाव को भी जानते हो, कुभाव को भी जानते हो । जब सब कुछ तुम जानते हो, भाव कुभाव को तो फिर यही निवेदन है कि 'पुरजन जननी भरत हित, होय सो कहढु उपाय ।' जो सबके हृदय में होगा वही ऐसा फैसला देगा । इसलिए मैं आत्मा अखंड, ज्ञान स्वरुप एक हूं। सबमें सबको प्रत्यक्ष हूं अप्रत्यक्ष नहीं हूं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रमाण है कि में आत्मा प्रत्यक्ष हूं। इस प्रत्यक्ष (में आत्मा) को प्रत्यक्ष करने के लिए किसी साधन की जरुरत नहीं पड़ती । अरे जो प्रत्यक्ष ही है स्वभावतः उसको प्रत्यक्ष करने के लिए साधन की क्या अपेक्षा है। अगर कोई चीज छुपी हो, कोई जीज न हो, तब उसको प्रत्यक्ष करने के लिए कोई न कोई साधन की जरुरत पड़े । जब मैं भूतकाल में प्रत्यक्ष, वर्तमान में प्रत्यक्ष, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति में प्रत्यक्ष, मूर्छा समाधि में प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष स्वरुप मुझ आत्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए साधन की क्या जरुरत है ? तो फिर जब मैं विना प्रयास के, बिना साधन के, तीनों अवस्था, तीनों काल में प्रत्यक्ष हूं तो फिर मुझ आत्मा से बढ़कर पदार्थ कौन हो सकता है। काल चला जाता है, देश चला जाता है, वस्तु चला जाता है, मगर देश काल वस्तु के अभाव में मुझ आत्मा का अभाव कभी नहीं होता क्योकि में आत्मा कालातीत हूं। काल जिसको न खा सके, काल जिसको न ग्रसे और जो काल का काल हो उसको कालातीत कहते हैं । सबेरे तुम सोकर उठे, कब ? पांच बजे । अब पांच बजे कहां गया? दरअसल काल कहते हैं समय को । पांच को खाया, छः को खाया, सात को खाया । तो इस तरह काल जो है, काल का कितना प्रवाह है कि आज दिन तक बड़े बड़े वैज्ञा- निकों ने काल का माप पत्र नहीं बना पाया। काल में कितनी दौड़ है, कितना वेग है इसका मीटर नहीं बन पाया । सरसर, सरसर काल चला जा रहा है, भविष्य वर्तमान हो रहा है। मुझे आत्मा का परिवर्तन नहीं है। तभी तो मैं प्रत्यक्ष हूं, तो में हूं, इसलिए में आत्मा प्रत्यक्ष हूं और एक को नहीं, सबको । इसके प्रमाण के लिए तुम्हें पोथी पत्रे की जरुरत नहीं है। अगर में अस्तित्वत्रान न होऊ, मुझ आत्मा का वजूद न हो, अगर में न होऊं तो तुमसे प्रश्न करेगा कि कौन शास्त्र में लिखा है कि में हूं ? इसलिए में आत्मा प्रत्येक्ष हूं । भूत, भविष्य, वर्तमान तीनकाल में, जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में, सर्वकाल में और सर्व अवस्थाओं में में हूं, में आत्मा प्रत्यक्ष हूं। ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण । अब अनुमान का क्या लक्षण है? कहते हैं ये पहाड़ अग्निमय है माने इस पर्वत में अग्नि है। क्या प्रमाण है, धुवां निकल रहा है, पर्वत से तो पत्ता लगता है।
जैसे यहां कोई नदी है और बारिश हुई नहीं पर नदी में पानी बढ़ गया है। इससे अनुमान होता है कि यहाँ पानी नहीं गिरा तो बारिश आगे हुई होगी वहां से पानी बहकर आया तो पानी बढ़ गया नदी में । ये अनुमान प्रमाण का प्रमाण है। अब लगाओ आत्मा पर । कोई बीमार जैसे हो गया, या ज्यादा बुखार आ गया या आपत्ति आ गई तो कहते हैं कि अरे राम रे ! मर गया। तो जो मर जायगा वो कहेगा ? अगर मैं मर गया तो, दादारे ! मर गया कौन कहेगा ? इस कथन से ही सिद्ध होता है कि में मुरता नहीं। अरे बाप रे मर गया । अगर मैं मर जाता तो कहता कौन कि अरे बाप रे मर गया । इससे अनुमान होता है कि में मरता नहीं । और यदि कहो कि साहब मैं तो नर्ह है। शरीर दिखता है, इन्द्रियाँ दिखाई देती हैं, मन भी दिखता है। सब कुछ दिखता है। तो इनको फीन देखता है? मन के आनेजाने को कौन देखता है ? इससे अनुमान होता है कि में हूं। ये दूसरी चीज़ है कि मैं नहीं दिखें। ये दूसरी चीज है। यहां तो अस्तित्व की सिद्धि की जा रही है। ये दूसरी चीज है, में क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, में कहां हूं, ये दूसरा सवाल है मगर हूं तो सही । साहब, मैं तो नहीं जानता कि में क्या हू । तो मैं नहीं होता तो नहीं जानता को कौन जानता । भैय्या, इसका नाम गलग्राही न्याय है। सब बातों के लिए और चीजों को सिद्ध करने के लिए तो प्रमाणो की जरुरत है, मगर मैं हूं इसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण को जरुरत नहीं है। अरे यहां बारिश नहीं हुई तो आगे हुई होगी । अनुमान होता है कि में हूं हर हालत में । साहब मैं तो नहीं जानता । ये प्रत्यक्षसार का विवेचन है। इससे अनुमान होता है कि में हूं। देखो - भगवान है। अव दूसरी युक्ति आ रही है। भगवान है, या भगवान नहीं है, ऐसा जो कहता है, इसको, भगवान के भाव अभाव को, ईश्वर है या नहीं है, इसको, बुद्धि स्वीकार करती है। ईश्वर है अथवा ईश्वर नहीं है, ये जो मान्यता है, ईश्वर है ये भी एक मान्यता है, ईश्वर नहीं है ये भी एक मान्यता है । तो ईश्वर के भाव अभाव का साक्षी, ईश्वर के हैं नहीं का ज्ञाता ईश्वर है, इसकी सिद्धी ईश्वर से होती है या मुझ आत्मा से ? बदलना नहीं । ये सुप्रीम कोर्ट है भैय्या । यदि कोई अनीश्वर- बादी आ जाए और आजकल निरीश्वर बादी बढ़ रहे हैं। वैसे तो नास्तिक सारा सँसार है। अस्तित्ववान पदार्थ को जो जानता है वही आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक है। खैर । कोई निरीश्वर आ जाए और नास्तिक अगर कहता है कि क्या ईश्वर है ? तो क्या कहोगे बसे ? रामायण गीता का प्रमाण देते हो कि लिखा है इसमें, तो मानता नहीं वो । क्योंकि प्रचार में सबसे लोहा लेना पड़ता है, हमको । वो लोग कैसे तार्किक होते हैं। उनको प्रमाण देने की जरुरत नहीं है। अगर पूछे कि क्या ईश्वर है ? तो कहो कि जी हां है। क्या प्रमाण है ? क्योंकि में हूं, इसलिए ईश्वर भी है। ईश्वर के भाव अभाव का साक्षी कौन होगा, इसको देखेगा कौन, इसका अनुभव कौन करेगा । तो में हूं, इससे अनुभव होता है कि में हूं इसलिए ईश्वर भी है। क्योंकि ईश्वर के भाव अभाव को में आत्मा ही सिद्ध करता हूं। देखो भैय्या जो नास्तिक है न, वो भी में का विरोध नहीं करता । ईश्वर का विरोध तो करता है मगर में का विरोध वह भी नहीं करता । अब प्रश्न होता है कि पुराने जमाने में राक्षसों ने भगवान का विरोध किया और तुम कहते हो जो निवि- रोध है वही भगवान है। मगर रावण, कंस जितने दैत्व हुए हैं, ये सभी विरोधी थे । तो फिर ये कथन गलत हुआ कि भगवान वही है जो निविरोध है। ये लोग जो विरोधी थे, काल्पनिक भगवान के विरोधी थे । वास्तविक भगवान के नहीं । तो काल्पनिक भगवान का कोई विरोधी होता है । कोई अविरोधी होता है । मगर जिसने उस आकार प्रकार को धारण किया, वह निर्विरोध है। तो नास्तिक भी शान्त हो जाता है। तो नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए यही निविरोध सिद्धांत है । अनुमान प्रमाण का ये प्रमाण दिया जा रहा है। में आत्मा पर। मैं प्रत्यक्ष हूं और प्रत्यक्ष होते हुए में न होऊं तो ईश्वर के है नहीं का साक्षी कौन होगा, शरीरादिक प्रपंच को कौन जानेगा। मैं क्या हूं, कैसा हूं, कौन हूं, ये अलग चीज है। मगर यहां तो अस्तित्व का बोध कराया जा रहा है। मैं हूं तो हूं, चाहे कैसे भी रहूं । चाहे देह रुप में मानो, चाहें स्त्री मानो, चाहे पुरुष मानो, चाहे कुछ भी सही। चलो देह ही सही। मैं क्या हूं, कैसा हूं, कौन हूं, कहा हूं, इसका विवेचन चौथे प्रमाण में होगा स्वानुभूति प्रमाण में। अभी तो अनु- मान प्रमाण बता रहे हैं। अरे भई इन्द्रियां न जाने मुझको । इन्द्रियां भले न जान सकें, मन बुद्धि चित्त भले न जान सके, वाणी भले न कह सके । ये तुम्हारे कहने से मान गया कि मैं हूं। मगर मैं कौन हूं, कैसा हूं। तो में हूं, तो इसको क्या नहीं जानता ? तो यह तो जानता है । मैं कौन हूं, कहां हैं, कैसा हूं, इसको जानना है । मैं को जानता है तो ये तो समझ गए कि में है ईश्वर के भाव को, अभाव को, शरीरादिक को सबको मै जानता हूं, इससे अनुमान प्रमाण सिद्ध है कि मैं जरुर हूं। ये तो समझ गए न? कि मैं हूं। हाँ, हूं। तो यहां सवाल पैदा होता है कि में क्या हूं? में कैसा हूं, में कौन हूं, में कहां हूं। भैय्या यदि इसको में जानू तो मैं ही नहीं। बहुत बारीक चीज है। बुद्धि खो जाती है क्योंकि मैं ही हो जाती है। वो निश्चय कौन करे । में क्या हूं, कैसा हूं, कौन हूं, इसका निश्चय करने के लिए जब वृद्धि चलती है तो में ही हो जाती है, उसका ये सारा प्रश्न हल हो जाता है। बुद्धि का मैं हो जाना, बुद्धि के सवाल का यही जवाब है। बुद्धि का बात्मा हो जाना, बुद्धि के सारे मसले का यही हल है। पाश्चात्य दर्शन और प्राच्य दर्शन में इतना अंतर है। वहां के विद्वान बुद्धि- बादी होते हैं। कहते कहते निश्चय करते करते उनकी बुद्धि जब खो जाती है, तब कह देते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। वहाँ पर भारतीय बेदान्त ताल ठोककर सामने आ जाता है। तो भारतीय वेदान्त कहता है- कि जो जानता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, वो है कि वो भी नहीं है ? मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, ये बुद्धि का सवाल है। इसको हल करने के लिए चलती तो है बुद्धि मुझ आत्मा के बिदीक । मगर वहां जाकर वह खो जाती है। क्या भी गया, कौन भी गया, कैसा भी गया में आत्मा ही हो जाती है। अब उसका वजूद हो तब तो आके बतावे कि कौन है, कैसा है, कहां है। अब सब खातमा हो गया तो बतावे क्या ? यही हाल वाणी का भी है। क्योंकि जो चला छूने को, छुवा गया। जानत तुहि तुमहि होजाई । ये बात है। और निगम ? निगमादिक जो है, निगम और आगम । ये भी अपने अपने दिमाग का फुजला निकालते है। तुम सत हो, तुम चित्त हो, कूटस्थ हो, व्यापक हो अखन्ड हो, पूर्ण हो, सब कहते । और बुद्धि ही वेद है, बुद्धि ही शास्त्र है। श्रुतियां स्मृतियों शास्त्र बुद्धिवाद हो तो हैं। जब बुद्धि ही खो गई, में कौन हूं, कहाँ हूं, कैसा हू, इन सवालों के हल में जब बुद्धि ही में आत्मा हो गई, तो ये सवालात खतम हो गए। तो बुद्धि के बनाये ये निगमागम सब खतम हो गए । रह गया विशुद्ध तत्व अब । मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, में कैसा हूं, तो बुद्धि अगर न खो जाय, तो 'मन समेत जेहि जान न वाणी' ये हार मानकर 'राम अतर्व्यवृद्धि मन वाणी' । भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से 'मत हमार अस सुनहु भवानी' । ये हमारा अनुभव है कहते हैं भगवान शंकर । ये स्वयं हमने अनुभव किया है कि भगवान राम मन बुद्धि का विषय नहीं है। राम ऐसा है, राम इस प्रकार है, ये कुछ नहीं । 'अतर्क बुद्धि मनवाणी तो'-
'प्रत्यक्षेणानुमानेन.... आत्म संविदा'
प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, निगम प्रमाण और स्वानुस्ति प्रमाण । निगम प्रमाण तो सुन ही रहे हो ।
'नान्तः प्रज्ञम् .... स विज्ञेयः'
निगम प्रमाण तो आज छः दिन हो गए देते । ये निगम प्रमाण ही तो हैं ।
अब चलो चौथा प्रमाण । स्वानुभूत्ति प्रमाण-आत्मसंविदा कहते हैं स्वाभूति प्रमाण को । स्वानुभूति प्रमाण-मैं क्या हूं, मैं कैसा है में कौन हूं, मैं कहां हूं? बुद्धि के अभाव में, बुद्धि के विगत हो जाने पर, देख।-बुद्धि का अभाव होना कहो, चाहे बुद्धि का विगत होना कहो, विगत कहते हैं नाश को । वृद्धि का अभाव चित्त का अभाव, पन का अभाव तो ये जाने कहां हैं ? जिसमें इनका भाव है, उसी में सवों का अभाव है । में आत्मा के अज्ञान से हो इनका भाव है और में आत्मा को जान लेने पर इन सबों का अभाव है। जिस तरह रज्जू के अज्ञान से सपें है और रज्जू के ज्ञान से सर्प रज्जू है। रज्जू के ही अज्ञान से रज्जू सर्प है और रज्जू के जान लेने पर सर्प ही रज्जू है। ऐसे ही में आत्मा के अज्ञान से मन बुद्धि चित अहकार देहादिक प्रपंच हैं और में आत्मा के ज्ञान से इन सबों का अभाव हो गया माने म हो गया। देखो - तद्वत, वही होता है जो तद्रूप होता है। यदि नदी जलवत् न हो, तो समुद्र में उसका मेल नहीं । तो अगर में आत्मा वृद्धि न होऊ तो मुझ आत्मा को छूकर बुद्धि आत्मा न हो । अगर मैं आत्मा शरीरादिक और सत रज तम यदि में आत्मा न होऊं तो मुझ आत्मा के साथ इनकी तल्लीनता न हो । इससे निर्विवाद सिद्धांत है कि मैं हूं। इनके रहने तक ही में ही हूं कि इनके अभाव में में ही हूं। बुद्धि अगर दिखाई देती है तव में ही हूं और जब बुद्धि का अभाव हो गया तो में हूं। शब्दादिक विषय यदि मुझ आत्मा से भिन्न दिखते हैं तब तो कहो में ही हूँ और इनमें और मुझमें भिन्नता की प्रतीति नहीं होती तो मैं हूं । मैं हूं इसकी अनुभूति के लिए ही तो उस दिन में का डंडा दिया गया था कि जब अनभ्यास के अभ्यास में बैठते हो तो यदि शब्दादिक विषय अपने आप से भिन्न प्रतीत होते हैं और इन विषयों की भिन्नता में ही हर्ष और शोक होता है तो फिर मैं ही हूं और नहीं होता तो में हूं। में ही हूं ये हथियार भिन्नता का नाशक है, भेद का नाशक है। जब भिन्नता की प्रतीति न हो तो फिर में हूं ये भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे में हूं इसको भी तो वाणी ही कह रही है कि में हूं और वाणी उसका कथन करती है, वृद्धि जिसको निश्चय करती है और जहां पर बुद्धि का बोध खो जाता है, तो बुद्धि का निश्चय कार्य, जब बुद्धि के निश्चय का अभाव हो गया तो वाणी किसको कहेगी । बुद्धि जिसका निश्चय करती है उसी का चित्त चितन करता है, मन मनन करता है, चक्षु इन्द्रो देखती है और वाणी उसी को व्यक्त करती है। तो मैं कौन हूँ, कैसा हैं, में क्या हूँ, कहाँ हूँ, ये बुद्धि का प्रश्न है, तो जब बुद्धि ही खो गई तो बुद्धि का निश्चय कार्य खतम हो गया । जिसका जो धर्म होता है, वह अपने धर्मों से भिन्न नहीं होता । चाहे निश्चय कहो, चाहे बुद्धि कहो । मनन कहो चाहे मन कहो, देखना कहो चाहे आंख कहो । और देखना है तो आँख है, आंख है तो देखना है। सुनना है तो कान है, कान है तो सुनना है । तो जिसका जो धर्म होता है, वह धर्मी रूप होता है। तो उसी तरह में हूँ तो जानना है, जानना है तो मैं हूँ । जैसे देखना ही नेत्र है, चिन्तन ही चित्त है, निश्चय ही बुद्धि है। उसी तरह जानना ही में हूँ। मैं क्या हूं, कौन हू, कैसा हूं, कहाँ हूं, बुद्धि के अभाव में, बुद्धि के न रहने पर, इनके अभाव में क्या मैं आत्मा का भी अभाव हो जाता है? नहीं होता तो मैं क्या कहता हूं ? बुद्धि के ही रहते तक ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है। जब बुद्धि का अभाव हो गया तो कहाँ गए । अगर कुछ कहते हो वाणी से तो सब गड़बड़ है। यही स्वानुभूति प्रमाण है । 'राम अतर्क्स बुद्धि मन वाणी' । इस अनुभूति में मैं हू । -शंकर सहज स्वरूप सम्हारा' । 'सहज विमल मन लागि समाधी' । बही सहज समाधि है। सब गायब हो गया । दिवाला चित्त हो गया । आनन्द मानन्द कर प्रसन्नम् । बुद्धि को जब जिन्दा करो तब । अरे जिसने मारा है, वही जिलावे। कहते हैं बड़े भारी भगवान बने हो भगवानतो मारता जिलाता है। एक भी तो मारो जिलाओ। यहां तो रात दिन मारा जाता है। वृद्धि कब की पैदा हुई । इसीलिए तो मैं शिव हूं। यही हकीकत है बाकी सब अफसाना है और जो कहानो होती है वो फर्जी होती है, झूठी होती है। कहानी और इतिहास में क्या फर्क है। कहानी का आधार घटना होता है और इतिहास का आधार पात्र होता है। तो बुद्धि का काम निश्चय, मन का काम मानना, आख का काम देखना, प्रपच का स्गरूप उत्त्पत्ति और विनाश, ये सब घटनायें रात दिन घटती रहती हैं, इसलिए ये सब कहानी है, अफसाना हैं। अगर कोई कहे कि कहानी का क्या लक्षण है तो यही बताना कि जिसका आधार पात्र हो वो इतिहास है । और घटना लेकर कहानी लिखी जाती है ।
'प्रत्यक्षेणा नुमानंन ……………………विचरेदिह'
इस प्रकार जानकर ससार में विचरना चाहिए । प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण-निगम प्रमाण और स्वानुभूति प्रमाण चारों प्रमाणों का विश्लेषण किया गया । इसलिए कि में प्रत्ययसार भगवान आत्मा हूं क्यो कि में प्रत्ययसार माने विश्वसनीय हू । हकीकत है तो में ही हूं। क्योंकि में जैसा शुरु में था वंसा ही में आखिर में रहूँगा और जो बोच है वह भी में ही हूं। जो पहले न रहे और बाद में न रहे और बीच में दिखाई दे वह प्रपंच है, माने वैतथ्य है। तो जो देहाधिक प्रपंच, सारा विश्व ये पहले नहीं था, अन्त में नहीं रहता, और वीच में प्रतीत हो रहा है इसलिए इसका नाम प्रपंच है, संमार है। और मैं आत्मा जैसा पहले था वैसे ही आगे रहूंगा. वैसे हो अब हूं। मुझ आत्मा में कभी परिवर्तन हुआ था, न है नहोगा। ये प्रपंच जो कोच में दिखाई देता है, प्रतीत होता है, मैं ही हूं, क्योंकि मुझ आत्मा से भिन्न प्रपंच की सत्ता नहीं है । प्रपंच प्रतीत होत है तब कहो में हो हूं और प्रपंच प्रतीत नहीं होता तो मैं हूं । प्रपंच की प्रतीति होने में मैं ही हूं। यहां तक बुद्धि है। और प्रपच प्रतीत न होने पर मैं हूँ। अगर कोई वस्तु संसार में जानने योग्य है तो मैं आत्मा ही हूँ। प्रपंच न देखने योग्य है न सुनने योग्य है ।
नान्तः प्रज्ञम् …………….. सविज्ञेयः
सप्तम दिवस का प्रवचन
(रविवार दिनांक १८ नवम्बर सन् १९७३ (समय १० बजे से १२ बजे सप्तम दिवस)
'ओभित्येदक्षर ………………….ओंकारेव'
नान्तः प्रज्ञम् .. ………………स विज्ञेयः
(पाठ)
नान्तः प्रज्ञम् .۰۰ ... ... स विज्ञेयः
इम मत्र में स्वरूप भगवान आत्मा के सभी विशेषण हैं। कल के प्रसंग में प्रत्ययसार का विश्लेषण किया यया । प्रत्ययसार उप- निषद की भाषा में कहते हैं विश्वसनीय पदार्थ को । जो विश्वास- पात्र हो उसको प्रत्ययसार कहते हैं। इसका विवेचन कल हो चुका है । प्रत्ययसार । देखो व्यवहार में भी कभी कभी किसी अपने बड़ आफीसर के नाम जब आवेदन पत्र कोई लिखता है, दरखास्त या एप्लीकेशन जो कुछ भी कहो तो भैया, व्योरा सब लिख लिया जाता है अथवा टाइप कर लिया जाता है तो सब के बाद में यह लिखा जाता है कि 'तुम्हारा विश्वास पात्र' । उसके बाद फिर क्या लिखा जाता है- तुम्हारा विश्वासपात्र 'मैं' । अब में के पीछे कोई न कोई पूछ लंगा दी जाती है। में मनोहरलाल, में यज्ञदत्त । तो मै के पीछे कोई न कोई पूछ काल्पनिक लगा देनी पड़ती है। असली जो विश्वास पात्र है, वो तो में ही हूं। क्योंकि शरीर भी विश्वास पात्र नहीं है, इन्द्रियां भी विश्वासपात्र नहीं है, मन बुद्धि चित्त भी विश्वाप्त पात्र नहीं हैं। तो फिर किसके लिए लिखते हो तुम्हारा विश्वासपात्र । - ये व्यवहारिक वेदान्त है। जब लिखने का मौका आता है तुम्हारा विश्वास पात्र तब लिखते हो में । और मैं का ही विवेचन हो रहा है। यहां पर एक और विशेषता है, जो कुछ लिखते हो सबकी टाईप हो जाती है, और तुम्हारा विश्वासपात्र भी टाईप हो जाता है लेकिन जहां में लिखना होता है तो में की टाईप नहीं होती क्योंकि मैं आत्मा तो सबको टाईप कर रहा है। ये जाग्रत है, ये स्वप्न है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो सारे प्रपंच की टाईप तो में आत्मा रात दिन करता हू तो मैं की टाईप करने वाला कौन है भैया, संसार में। तो मैं का टाईप नहीं होता। में आत्मा मन वाणी का विषय नहीं तो टाईप में कैसे आयेगा तो जब में लिखने का टाईम आता है तो कच्ची स्याही से, पेन निकालकर लिखा जाता है। में पढ़ा नहीं हूँ, तो दूसरे से भी नहीं लिखा सकता क्योंकि मैं का लेखक तो में हो हूं और दूसरे से लिखवा लोगे तो जुर्म है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो अंगूठे का निशान भी मेरा ही होगा। व्यवहार में भी देखो तो में आत्मा की महिमा चारों तरफ फैली हुई है इसलिए मुझ आत्मा को प्रत्ययसार कहते हैं ।
आगे का विशेषण आता है- 'शान्तम्', 'प्रपन्चोपशमम्' । मुझ भगवान आत्मा में प्रपंच का उपशम है। यानी मुझ आत्मा में प्रपंच तीनकाल के अन्दर है ही नहीं। तो प्रपंचोपशयम् । फिर उसके बाद शान्तम् । जब प्रपंचोपशमम् में प्रपंच की निवृत्ति है, प्रपंच है ही नहीं मुझ आत्मा में तो किसकी अपेक्षा से मैं हूं कहे। क्योंकि तू की अपेक्षा से मैं हूं और मैं की अपेक्षा से तू है। तो प्रपंच नहीं तो तू नहीं और तू नहीं तो मैं नहीं । इसलिए 'शान्तम्' । प्रपंच का सर्वथा मुझ आत्मा में अभाव है। प्रपंच है ही नहीं ।
आदावन्ते चयन्नास्ति वर्तमानेऽपितत्तथा ।
वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लकित्त्ताः ।६।
गौ. पा. का. वैतथ्य प्रकरण
जो आदि में नहीं, अंत में नहीं, मध्य में जो प्रतीत होता है यह भी नहीं, ये तो वैतथ्य है। है के समान दिखता है परन्तु विचार करने पर नहीं मिलता । आदि में याने शुरुआत में नहीं और अत में नहीं और जो बीच में प्रतीत होता है, ये भी नहीं । इसलिए यहां पर विशेषण दिया है भगवान आत्मा का प्रपचोपशमम् । प्रपच का उपशम है माने प्रपच की निवृत्ति है। जब प्रपच नहीं है तो फिर प्रपंच के ही अंदर तो में तू है। जब तू नहीं तो में भी नहीं । अब जो कुछ है उसके लिए कहते हैं शान्तम् । शान्त महासागर' ।
शान्ति से शान्त की अनुभूति है कि शान्त से शान्त की अनुभूति है अरे भई, जब प्रपंच की निवृत्ति है, प्रपंच तीन काल में है ही नहीं, प्रपंच क्या है ? जो अपने आधार को ढांके उसका नाम प्रपंच है। डंडा क्या है ? अरे जो लकड़ी को ढांके। लकड़ी का जो आवरण है, लकड़ी को जो आच्छादित करता है, उसका नाम डंडा है। जो सोने को ढांकता है, उसका नाम आभूषण है। तो प्रपंच किसको कहते हैं? • जो अपने आधार को ढांके, तो प्रपंच का आधार में आत्मा हूं तो मैं आत्मा को जो ढंकने वाला है, वो प्रपंच, माया है। यहां पर प्रश्न होता है कि क्या दरअसल में आत्मा ढंकता हूं ? जी नहीं उस वक्त प्रपंच से भगवान आत्मा मैं ढांका जाता हूं, ये उस वक्त कहा जाता है जब कोई दूसरा ढांकने वाला हो । जब कोई दूसरा मुझ आत्मा को ढांकने वाला हो तब तो कहा जा सकता है कि में आत्मा प्रपंच से हँकता हूं । प्रपंच की सत्ता मानकर ।
ढँकना क्या है, और उघड़ना क्या है ? प्रपंच है, ऐसा मानना ही ढकना है। और प्रपंच को जब जाना तो यही प्रपंच का उघरना है। प्रपंच है, देह है, ऐसा मानना ही देह है। देहादिक प्रपंच है ऐसा मान लेना ही देहादिक प्रपंच है । और ये मानना ही मुझ आत्मा का ढक्कन है। और देह को जब जानने चला तो यह न मिला, यही उघरना है। बड़ा सुन्दर खेल है। बड़ा विचित्र खेल है। तो मानने में देह है, जानने में में हूं। मानने में संसार है, जानने में मैं हूं, जैसे मानने में सर्प है और जानने में रज्जू है, उसी तरह मानने में संसार प्रपंच है और जब जानता हूं उस माने हुए प्रपंच को जब जानने चाहता हूं तब प्रपंच नहीं मिलता । नहीं दिखता तो प्रपंच का जानने वाला ही में आत्मा रह जाता हूं। प्रपंच हो जाता है वैतथ्य और में रह जाता हूं तथ्य वास्तविक । हां तो फिर तथ्य ही रह गया तो "शान्तम्" । मानने से प्रपंच और जानने से प्रपंचोपशमम् प्रपंच की निवृत्ति तो तभी होगी, जब प्रपंच को जानोगे । तो प्रपंच को जान लेने पर वास्तव में मुझ आत्मा के सिवाय कोई दूसरा अस्तित्व रहता नहीं, इसलिए मुझे आत्मा को भगवती श्रुति प्रपचोपशमम् विशेषण देती है, मैं अपने आपको प्रपंचोपशमम कहने में भी तो समर्थ नहीं हूं। ये तो श्रुति कहती है। ये विशेषण, जितने भगवान आत्मा के हैं, जिनकी व्याख्या हो रही है, सब श्रुति के बनाये हुए विशेषण है। श्रुति को जैसा जैसा अनुभव होता गया, उसी तरह वह आत्मा को विशेषण देती गई । परन्तु साक्षात् कथन करने में स्वस्वरुप का, श्रुतिं भी समर्थ नहीं है, इसलिए 'शान्तम्' ।
अभी बीच में एक प्रश्न किया था, हल करना बाकी रह गया है। शान्त से शान्ति है कि शान्ति से शान्त है। देखो, समझो, यानी शान्ति से शान्त का अनुभव होता है (शान्त में आत्मा) या शान्त से शान्ति का अनुभव होता है । एक । एक मर्तबे और सुनो । यानी साफ शब्दों में ये है कि प्रपंच की निवृति हो जाने पर स्वस्वरुप आत्मा (निवृति भी कठिन शब्द आ गया, सब न समझग ।)
देखो - अन्धकार में जो सांप दिखाई देता है तो सप के नाश हो जाने पर, रज्जू का ज्ञान होता है कि रज्जू को जान लेने पर सर्प का नाश होता है । सर्प के नाश हो जाने पर, सर्प के मर जाने पर रज्जू का ज्ञान होता है कि रज्जू को जान ले तब सर्प का नाश हो जाता है। रस्सी के जान लेने पर ही सर्प की निवृत्ति होती है। ठोक है, और निवृत्ति के ही माने शान्ति है । उसी तरह प्रपंच की निवृत्ति का नाम शांति है। तो फिर भैय्या, प्रपंच के अभाव हो जाने पर माने प्रपंच की निवृत्ति हो जाने पर शान्त पद का अनुभव होता है या शान्त पद की अनुभूति हो जाने पर शान्ति की अनुभूति है यानी शान्ति से शान्त है कि शान्त से शान्ति है ? शान्त से शान्ति है, और अगर कहें, यदि हम ऐसा कहें कि शान्ति से माने प्रपंच की निवृत्ति हो जाने पर प्रपंचाधार में आत्मा हूं, शान्त उसका अनुभव • होता है, तो बिना शान्तपद स्व स्वरूप के जाने प्रपंच की निवृत्ति होती नहीं तीनकाल में, असंभव है।
जैसे कि रज्जू को न जाने, रज्जू का ज्ञान न प्राप्त करें और बिना रस्सी के जाने सर्प का मारने की कोशिश करना, रज्जू से सर्प यदि सर्वथा भिन्न है तब तो रज्जू को बिना जाने ही सर्प नाश किया जा सकता है, किसी pi किसी कोशिश से और जब रज्जू ही सर्प है तो बिना रज्जू के जाने सर्प का नाश नहीं होता । तो उसी तरह यदि में आत्मा से संसार प्रपंच भिन्न है तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है संसार का नाश करो, और सब कर ही रहे हैं। ससार से तरने का उपाय लोग कर रहे हैं। अरे संसार है अथवा नहीं है इसके जानने के लिए कोशिश नहीं करता । तरने का उपाय करता है। जबकि रज्जू ही सर्प है, उसो तरह में ही प्रपंच हूँ. में आत्मा ही प्रपंच हूँ और यो कहो कि मुझ आत्मा का ही पर्या- यवाची नाम है। जबकि में ही प्रपच हूँ तो मुझ आत्मा से प्रपंच की सत्ता भिन्न नहीं है तो संसार सागर से पार होने के लिए और कोई उपाय न करके सबसे पहले भगवान स्वरूप आत्मा को जान लेवे । तो रज्जू को जान लेने पर वह ससार सागर से तर जाता है माने संसार नाश हो जाता है । और तरोगे किससे ? इसी लिए कहा जाता है, भजन करोगे तब न तरोगे और न करोगे तब न तरोगे । इसीलिए भजन करो । ये मस्तों के लतीफे है भैय्या ! भजन करोगे तब न तरोगे और न करोगे तब न तरोगे । तो फिर भजन क्यों करें ? अरे भजन करोगे तभी तो तुमको मालूम होगा । जब भजन करोगे तब इस रहस्य का पता लगेगा। और तरना किसको ? मृग- जल समुद्र को तरना जिस तरह, अरे उसी तरह संसार से तरना । तो इन दृष्टांतों से, इन उदाहरणों से, इन युक्तियों से यही सिद्ध होता है कि मुझ आत्मा में प्रपंच का सदा उपशम है। इसलिए ! जिज्ञासुओं ! एक प्रश्न होता है । स्वामी जी ! वस्तु का बोध हो जाने पर (वस्तु माने आत्मा) माने स्वस्वरूप भगवान आत्मा का बोध हो जाने पर भी प्रपंच क्यों दिखता है ? ये तुम्हारी शंका है। हमारी शंका नहीं है। इतने दिन से सुन रहे हो कि स्वस्वरूप के सिवाय प्रपंच तीन काल में नहीं है। मगर ये सुनकर के भी, जान- कर के भी, प्रपंच क्यों दिखता है । तो भैय्या, जो दिखता है, वह प्रपंच है । स्वामी जी! रज्जू को देख लेने पर सर्प क्यों दिखता है ? ऐसा ही है न ! रज्जू को जान लेने पर सर्प क्यों दिखता है ? फिर तुमनें रज्जू को देखा ही नहीं। अगर सर्प दिखता है तो रज्जू का दर्शन नहीं हुआ । हां ये कह सकते हो कि रज्जू का दर्शन कर लेने में अंधकार में जो भय कंपन था, अरे साँप तो था ही नहीं जी। पता नहीं, मुझे कैसे भ्रम हो गया, तो उजाले में भी थोड़ा धकधक होता रहता है । तो उसी तरह बोध हो जाने में भी. प्रपच तो नहीं रहता लेकिन वो धड़कन जो है, इसलिए अनभ्यास का अभ्यास करना बहुत जरूरी है । धड़कन निकालने के लिए। ऐसा न हो कि धड़कने बढ़ जाए । और धड़कन पहले तो नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में ही धड़कन आई है। तो ऐसा न हो कि फिर हार्टट्कल होने लगे । इसलिए हम तुम लोगों में जोर दे रहे हैं। जो जाने हो न, वो ज्ञान अनभ्यास से पक्का हो जायेगा । धड़कन भी निकल जायगा । वो अनादिकाल का संस्कार है। संसार कब से है, कोई तिथी तारीख तो है नहीं। अब निकल तो गया है जो लौट के नहीं आएगा, मगर वो जो पूर्व का संस्कार रह गया है, उसको निकालने के लिए अनभ्यास का अभ्यास बहुत जरूरी है। इस प्रकार की शंका होना स्वाभाविक है। और कोई कोई इस शंका से बचा हो नहीं तो सबको शंका होती है। वो जो अनभ्यास करते हो वो ज्ञान का अनुष्ठान है। जो अनुष्ठान करने से जिस काम के लिए अनुष्ठान किया जाता है वो काम सिद्ध होता है। अनुष्ठान की यही सिद्धी है कि वो संस्कार आगे न रहे, उसकी स्मृति न हो, उसके लिए अनभ्यास करना बहुत जरूरी है। स्कूल कालेज का जो शिक्षक होता है वो तो यही चाहता है कि हमारे क्लास के जो छात्र हैं वो सेन्ट परसेन्ट नम्बर से पास हो जाय, एक भी फेल न हो। अनादि काल का जो संस्कार पड़ा हुआ है हृदय में वो निकल जाए। तो जब संस्कार निकल जाते हैं, प्रपंचों पशम के बाद, तो 'शान्तम्' । वाह ! तुम्हारे संस्कार जब निकल जायेंगे तो दूसरे के संस्कार भी तुम्हारे कथन से निकल जायेंगे । प्रपँचोपशम मुझ भगवान आत्मा में प्रपंच की निवृत्ति है। तीन काल में है ही नहीं । देखो इस शहर का नाम रायपुर है, मगर रायपुर किसी ने देखा नहीं । अब तुम कहोगे-स्वामी जी ! आँख से तो हम देख रहे हैं रायपुर और तुम कहते हो कि नहीं है रायपुर । जिसका नाम तुमने रायपुर रखा है। रायपुर ढूंढ़ने चलोगे तो रायपुर नाम का शहर न मिलेगा, तो फिर जो ये दिख रहा है तो रायपुर का देखने वाला में दिख रहा हूँ कि रायपुर दिख रहा है ? में दिख रहा हूँ। यही प्रपंच की निवृत्ति है। प्रपंचोपशम । जब रायपुर नहीं तो जिला नहीं, तहसील नहीं, और भारत वर्ष नहीं । किसी भी चीज को देखने चलो तो मैं ही रह जाता हूं । आभूषण तलासो तो सोना ही मिलता है। किसी भी चीज को देखने चलो तो सिवाय अपने आप के कोई चीज दिखती नहीं है। में ही इसका देखने वाला हू और में ही ये दिख रहा हूं।। अपने आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। अब इस प्रकार से जान लेनें पर प्रपंच की निवृत्ति तो हो गई, रायपुर तो गया, मगर पुराना जो संस्कार अनादिकाल का जो बैठा है वो रह जाता है । अरे भई टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को जला दो, तो जल जाती है मगर उसकी सूरत संकल नहीं जाती, मगर वो बंधन का कारण नहीं होती । तो उसी तरह भैय्या, प्रपंच तो जल गया, उपशम हो गया, अब उसका जो टेड़ा मेढ़ा आकार है, तो आकार दिखता है, तो है तो भस्म ही, राख ही है । इसलिए प्रपंचोपशम । ये प्रपंचोरशन का विश्लेषण हो रहा है। जब प्रपंचोपशम तो उसके बाद 'शान्तम्' ।
कैसे कैसे सुन्दर महारानी श्रुति ने क्रमशः विशेषण दिया है। शान्तरम् पहले नहीं कहा, प्रपंचोपशम के बाद शान्तम् कहा । वाह भाई वाह ! अरे जला शान्तरम् तो जो शान्त है वही शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण । शिव माने कल्याण का है । तो प्रपंचोपशम, शान्तम् । प्रपंच निवृत्ति का संस्काराभाव का नाम ही शान्तपद है । प्रपंच की निवृत्ति का जो संस्कार, प्रपंच पहले था, और ज्ञान होने से अब निवृत्ति हो गया, इसके अभाव का नाम शान्त पद है । प्रपंच निवृत्ति का, संस्काराभाव का नाम है शांतपद । माने पहले प्रपंच था, पहले संस्कार था और बोध होने पर संसार निवृत्ति हो गया, यह जो संस्कार है संस्कार माने स्मृति । तो प्रपंच निवृत्ति के संस्काराभाव का नाम है। क्यों भैय्या, नदियां समुद्र में पहुंचकर, नदियाँ समुद्र को जानकर, नदियों की हो गई निवृत्ति । नदियों का अस्तित्व ही मिट गया, तो यह याद कौन करे कि आज के पहले मैं गंगा यमुना थी और अगर इसकी याद है तो समुद्र हुई नहीं । समुद्र प्राप्त नहीं की उसने, अगर पूर्वा पर को उसको याद है कि पहले में नदी थी और आज समुद्र हो गई। अगर यह याद है तो वह नदी ही है, समुद्र नहीं भई । ता, पहले नदी थी, अब समुद्र हो गई, उस नदी का पूर्व का संस्कार है, पूर्व की याद है उसको । और जब नदी ही न रही तो संस्कार कहाँ से और संस्कार नहीं तो समुद्र कहां । क्योकि नदियों ने ही मिलकर समुद्र नाम रखा, जब नदियां ही नहीं तो समुद्र कौन कहे ? अब जो रह गया वो न नदी है न समुद्र है। शान्त है। प्रपंच के ही अन्दर उपदेष्टा, उपदेश, उपदेश्य, बोध, अबोध, ज्ञान, अज्ञान है। और जब प्रपंच की निवृत्ति हो गई तो प्रपंच के अन्दर जो थे सब थे, इनका अत्यन्ताभाव हो गया । इन सबों को लेकर प्रपंच कहा जाता है । स्वदेश से देखो तो क्या तुमने कुछ पाया। कुछ तुमको मिला है या किसी ने तुमको अनुभव कराया है ? नहीं। इसलिए शान्तम् । क्या दिया, किसको दिया, क्या मिला, कहां से मिला, कब मिला, कुछ नहीं । क्योंकि शान्तम् । ये ही नारायण देश है। इसी का नाम परमपद है। ये ही कृतकृत्य पद है और यही-
पुरुषार्थ शून्यानी गुणानी प्रतिप्रसवः कंवल्पं
स्वरूप प्रतिष्ठावा चितिशक्तिरिति ।
पातंज्जलयोग दर्शन कैवल्यपादसूत्र ३४
ये ही स्वरूप की प्रतिष्ठा है अनुष्ठान सिद्धि ।
'उपजा ज्ञान बचन तब बोला'
सुग्रीव ने कहा-भगवान राम से ।
'उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउअडोला बड़ा चंचल था महाराज, ये मन । रात दिन हवाई महल बनाता रहता था, अडोला हो गया । तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को जानकर अडोला हो गया । जाय कहां? क्योकि प्रपंचोपशमम् । सागर म गल गया ये । जैसे पुतली लौन की सिन्धु थाह गइ लेन ।
प्रपंचोपशमम्, शान्तम् शिवम् अद्वैतम् । में आत्मा प्रपंचोपशम हूं, शान्त हूं, मै पहले बद्ध था, अब मुक्त हुआ में पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हुआ, में पहले जीव था, अब ब्रह्म हुआ । । ये सब संस्कार हैं। सब विकल्प हैं। पूर्वापर की स्मृति का अभाव ही संस्- काराभाव है माने सस्कारों का अभाव है। संस्काराभाव हो शान्त पद है और श्री मानसकार के शब्दों में पूर्वापर की स्मृति का अभाव ही अविद्या की ग्रन्थि खोलना है। उसी ग्रन्थी को खोलने के लिए बुद्धि बैठती है । अहब्रह्मास्मि के बाद । यही अविद्या की ग्रन्थि खोलना है। क्यों जी ! जीव को प्रपंच दिखाई देता है कि भगवान को ? अरे क्या सूर्य को भी अन्त्रकार दिखता है ? क्या इस प्रकाश को भी अंधकार दिखता है कभी ? तो अगर मुझ आत्मा को प्रपच दिखता है तो में आत्मा नहीं। मैं अभी जीव ही हूं। जीव को प्रपच दिखता है न कि भगवान आत्मा को । तभी तो प्रपंचोपशमम् हूं । आत्मा में प्रपंचाभाव है। स्वस्वरूप भगवान आत्मा में देहादिक प्रपंच का अभाव है। बयो अभाव है ?
सूर्य में जिस तरह अंधकार का अभाव है। हां जीव को दर्शन होता है प्रपंच का । मगर आत्मा को प्रपंच का दर्शन नहीं होता ।’ अब बैठे बैठे ही अनुभव करो न, अपने को कुछ न मानकर, में का मैं ही जानकर देखो, क्या प्रपंच दिखता है ? अगर प्रपंच दिखता है तो मैं नहीं और मैं हूं तो प्रपच नहीं। जैसे सूर्य को अन्धकार का दर्शन नहीं होता उसी तरह मुझ आत्मा को प्रपंच का दर्शन नंहीं होता तो अगर मुझको प्रपंच दिखता है तो में आत्मा नहीं हूं क्योंकि प्रपच जीव कल्पित है। कहना, सुनना, ज्ञान, अज्ञान ये सब प्रपंच के अन्दर है। तो गोया ये जीव कल्पित है। तो जीवभाव में इनकी प्रतीति होतो है, आत्मभाव में नहीं होती। मैं हूं-ये शान्त पद की अनुभूति कराई जा रही है। मै हू- इस देश से अब देखो कुछ दिखता है क्या ? और दिखता है तो मैं दिखता हूं कि मुझसे भिन्न दिखता है ? इस देश से माने अपने देश से, स्वदेश से, आत्मदेश से, तब तो मैं प्रपंचोपशम् होऊंगा । अरे रज्जू देश में सर्प है कि सर्प देश में सर्प है? सप देश में सर्प है। हो गया फिर। में हूं, इस स्थान से देखो, अपने देश से देखो मैं को कुछ भी मानना भगवान में कलक लगाना है। तो फिर में देश से, प्रपंच नहीं दिखता, तो इस लिए जो म प्रपचोपशम् हु । जब प्रपचोपशम हूं तो शान्तम् । प्रशान्त महासागर । और जब में आत्मा शान्त हूं, तो शिवम् । में शित्र हूँ । अब यहाँ पर डूब जाओ । में शिव हूं । शिवम् । अद्वैतम् । में भेदरहित है, द्वैतरहित है। अंगद ने क्या कहा था रावण से-
'सुन सठ होय भेद मन ताके,
*श्री रघुवीर हृदय हि जाके ।।
अरे ! रघुवीर का अनुभव करके भो भेद रहे। और हृदय में भेद • का निवास होगा उस हृदय में रघुवीर का निवास नही होगा ।
'सुन सठ भेद होय मन, ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके ।।
मोह किसको होता है- सुन मुनि मोह होय मन ताके, जान विराग हृदय नहि जाके । ये भगवान विष्णु ने कहा था नारद को। जब विवाह करने का पिशाच चढ़ा था सिर पर । 'सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहि जाके ।'
कहते है संसार में इतने हितैषी हैं । जननी, जनक, गुरू, बन्धु, सुहृद, पति सब प्रकार से हितकारी होते हैं, ये अनहित नहीं चाहते, हिषषो होते है। हे राम । तुम तुलसी के सब कुछ हो । तो तुलसी का ये ही विनय है तुमसे कि द्वैतरूप तमकूप में पडू नहीं । अव 'भविष्य में द्वैत रूप कूप में, अन्धकार में न पडू । भगवान कृपा 'कीजिए। तो भैया भगवान शिव आत्मा अद्वत है। दूसरा कोई नहीं । अरे अदबाहियो ! अपने को भगवान से अलग मानने वालो ! तुम जिन्दा कैसे हा ? तुम स्त्री का वियोग नहीं सह सकते, दूकान का • वियोग नहीं सह सकते, स्त्री का वियोग, पुत्र का वियोग तुम नहीं सह एकते । और भगवान के वियोग में जिन्दे हो ? शर्म है। और फिर भी भगवान के नक्त कहलाने के अधिकारी मानते हो ? ये जो भेद है। ये भेद तुम मानते किसमे हो ? भगवान यदि है तो भेद- रहित है। भेद को सिद्धी भगवान में नहीं होती । भगवान अभेदरूप है। तिनका तिनका भगवान है भगवान से अलग कोई चीज है हो' नहीं। कहां भेद लगाए बंड हो । इसलिए अद्वैतम् ।
नान्तः प्रज्ञम् ......स विज्ञेयः ।
इसी अद्वैत विशेषण पर ही इस मंत्र का उपसंहार है।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद, पूर्गात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिष्यते ।।
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! ! शान्तिः !!!
स्व० पं० कृष्णकुमार शर्मा के प्रति संवेदना के दो शब्द
गुरुनैष्ठिक स्वर्गीय पं. कृष्णकुमार शर्मा अध्यापक प्राथमिक शाला दुर्ग की स्मृति आज इस पुस्तक प्रकाशन के अवसर पर बरवश आ रही है चूंकि इस पुस्तक की प्रति- लिपि सुन्दर अक्षरों में आपने बड़ी लगन के साथ की थी । जिसे पढ़कर मुक्त सत्संग मंडल दुर्ग के सत्सगियों का ध्यान इस पुस्तक के महत्व की ओर आकर्षित हुआ था आज उनके अभाव में हम उनका स्मरण करते हुए उनकी अमर आत्मा की शान्ति एवं दुखी परिवार के लिये सुख-शान्ति हेतु नारायण रूप सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं। आपका स्व- र्गवास दिनांक ७/८/७४ को हृदयगति रुकने से हो गया था।
विनीत
'मुक्त सत्संग मंडल दुर्ग' 3