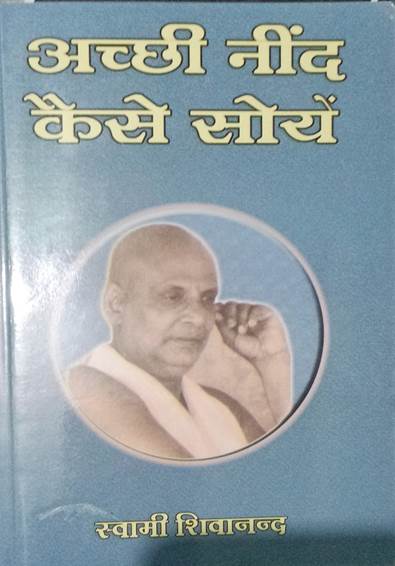
अच्छी नींद कैसे सोयें
'HOW TO GET SOUND SLEEP'
का हिन्दी अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती
अनुवादिका
शिवानन्द राधिका अशोक
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर – २४९ १९२
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण :२००५
द्वितीय हिन्दी संस्करण :२०१३
तृतीय हिन्दी संस्करण- :२०१६
(१,००० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
HS 11
PRICE : ₹70/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए
स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त
फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर- २४९१९२,
जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित।
For online orders and Catalogue visit: disbooks.org
|
जिन्हें नींद नहीं आती हो तथा समाधि के आकांक्षी जनों के लिए
|
|
दृष्टि को रूपान्तरित करें, इन्द्रियों को अन्तर्मुखी करें, मन को स्थिर करें, समाधि का आनन्द उठायें ।
|
श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज को आधुनिक रोग, जिसे अनिद्रा कहते हैं, से पीड़ित अनेकों लोगों के ढेरों पत्र नित्य आते थे।
यह स्थिति निःसन्देह आधुनिक भौतिक सभ्यता के कृत्रिम जीवन, भावनात्मक स्थिति तथा मानव की नाड़ी शक्ति के अत्यधिक बहाव के कारण उत्पन्न हुई है। परन्तु मात्र कहने से ही तो समस्या का समाधान या कष्ट का निवारण नहीं होता।
इसलिए यह पुस्तक श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने विशेष रूप से अनिद्रा से पीड़ित जनों की सेवा हेतु लिखी है। श्री स्वामी जी ने अलग-अलग प्रकृति के लोगों के लिए अलग-अलग विधियाँ बतायी हैं। जिन्होंने भी स्वामी जी की आध्यात्मिक विधियों को अपनाया, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई प्यासा एक गिलास पानी को खोज रहा हो और उसे अमरत्व प्रदान करने वाला घड़ा भर अमृत मिल गया हो।
यह पुस्तक अनिद्रा को ही दूर करने में सहायक नहीं होगी, प्रत्युत् यह को अज्ञानता की नींद से जगायेगी और उसे जाग्रत निद्रा की सर्वोच्च मनुष्य स्थिति समाधि या निर्वाण हेतु प्रेरित करेगी।
- द डिवाइन लाइफ सोसायटी
प्रस्तावना
श्वसन क्रिया के बाद नींद जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि श्वसन क्रिया जीवन को चलाती है, तो निद्रा जीवनी-शक्ति को वह आवश्यक अन्तराल प्रदान करती है जिससे शरीर की क्षति पूर्ति हो सके। यदि श्वसन क्रिया से जीवन का संरक्षण होता है, तो निद्रा से दैनिक कार्यकलापों में व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति होती है। यदि श्वसन क्रिया सभी प्राणियों में स्पन्दित होने वाली शक्ति का संकेत है, तो नींद अचल सुप्त यथार्थता हेतु आधार प्रदान करती है। यदि श्वसन रूपों की अनन्त विभिन्नताओं में प्रकट होता है, तो नींद अस्तित्व की अनिवार्य एकता का वर्णन हमारे समक्ष करती है। यदि श्वसन हमारे चारों ओर व्याप्त दिव्य ऊर्जा के स्रोत से, हिरण्यगर्भ से जीवन-शक्ति और ऊर्जा हमें ला कर देता है, तो नींद इनको हमारे अन्दर स्थित आत्मा से ला कर देती है। इस प्रकार श्वसन और निद्रा—दोनों ही आत्मा की अन्तर्वती अवस्था और श्रेष्ठता, सभी प्राणियों में व्याप्त वह सत्यता जो हमारे अन्दर है, विभिन्नता के मध्य एकता, वह अचल यथार्थता जो तत्क्षण अनन्त गति को प्राप्त हो सकती है तथा उस एकमात्र ईश्वर को जिसके द्वारा श्वसन और निद्रा अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, हमें दिखाती हैं। उस ईश्वर को नमन, उस पराशक्ति को प्रणाम जो इस संसार को चलाती हैं। उस निद्रा देवी को प्रणाम जो अचेतन अवस्था में आपको लोरी सुनाती है, जिससे आप अगले दिन के काम के लिए जीवनी-शक्ति प्राप्त कर सकें।
निद्रा बहुत से विशिष्ट सत्यों के लिए सूत्र प्रदान करती है। यह गुप्त रूप से प्रकट करती है कि आत्मा निःसन्देह एक सदृश और एक है। यहप्रकट करती है कि आत्मा समस्त कष्टों से परे और यह कि आत्मा एक शुद्ध आनन्द का पुंज है। निद्रा आपको यह बताती है कि जाग्रत अवस्था के समस्त अनुभव तथा (स्वप्नावस्था के विस्तार के अनुभव भी ) कम या अधिक कष्टप्रद होते हैं। गहन निद्रा में अनुभूत किये जाने वाले सुख तथा उसके सदृश अनुभव आपको किसी भी प्रकार के भौतिक अनुभव में नहीं प्राप्त होते। गहन निद्रा में मात्र एक ही दोष है (जो कि सारी विभिन्नताओं का कारण है), वह यह कि आप इसमें अपनी आत्मा के प्रति जाग्रत नहीं रहते। तुरीयावस्था सुषुप्ति के सदृश ही होती है; उसमें सबसे जीवित भिन्नता यह है कि तुरीयावस्था में आप आत्मा के प्रति चैतन्य रहते हैं। किन्तु यदि अनुभवों से जुड़े अन्य रूपों को देखा जाये, तो वे बिलकुल एक जैसे हैं। दोनों में से किसी भी अवस्था में दर्द की कोई अनुभूति नहीं होती।
दोनों ही अनुभव सभी के लिए एक प्रकार के और सामान्य हैं। किन्तु ऐसा जाग्रत अवस्था के अनुभवों के साथ नहीं है। विषय-वस्तुएँ सभी को एक-समान सुख नहीं देतीं, न ही वे एक मनुष्य को प्रत्येक बार एक-सा सुख प्रदान करती हैं। विषय-वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुख वास्तव में दुःख ही हैं।
कोई भी अनुभव जो मन को बहिर्मुखी बना कर मन और इन्द्रियों के संसर्ग पर प्रभाव डालता है, वह कष्ट ही है। कोई भी अनुभव जो मन को अपनी आत्मा की ओर ले जाता है, वही सच्चा सुख है। चेतना की दो अवस्थाओं गहन निद्रा की अवस्था और समाधि में मन स्वयं को इन्द्रियों और उनके विषयों से पृथक कर लेता है। यद्यपि स्वप्नावस्था में मन प्रत्यक्षतः इन्द्रियों और उनके विषयों से नहीं जुड़ा रहता, तो भी वह अपने आनन्दोपभोग हेतु स्वयं की वासनाओं की सहायता से स्वप्निल वस्तुओं की रचना करके उनसे खेलता रहता है। मन इस समय भी जाग्रत रहता है या अन्य शब्दों में यह इसके स्वयं के एकीकृत केन्द्र से दूर विषमता के क्षेत्र में
अभी भी विद्यमान रहता है। वह मनुष्य जो कई प्रकार के स्वप्न देखते हुए सारी रात बिस्तर में करवट बदलते हुए बिताता है, जब जागता है तो उतना ही अप्रसन्न रहता है जितना कि वह व्यक्ति जो जागृत अवस्था में बुरी तरह असफल रहा हो।
जाग्रतावस्था में मन इन्द्रियों से जुड़ा रहता है, चाहे अनुभव स्पष्ट रूप से कष्टप्रद या सुखदायक हों। उदाहरण के लिए पैर में काँटा चुभने के कष्टप्रद अनुभव को लीजिए। क्या होता है? तुरन्त इससे जुड़ा संवेदन अंग मन को पुकारता है — "हे मन! देखो, कोई मेरे भीतर प्रविष्ट हो गया है और मुझे दुःख दे रहा है।" मन तुरन्त उस स्थान पर जा कर उसका निरीक्षण करता है। और उपयुक्त अंग को उस काँटे को बाहर निकालने का आदेश देता है। यहाँ मन अन्तरात्मा से बहुत दूर रहता है, इसी कारण हमें दर्द की अनुभूति होती है।
आनन्ददायक अनुभव में इन्द्रियाँ प्रसन्नता से चीखती हैं— “अरे मन ! देखो, क्या ही आश्चर्यजनक वस्तु है।" यह ऐसा अनुभव है, जो इन्द्रियों को रुचिकर है। इसलिए मन उस स्थान को नहीं जाता, इसके विपरीत वह उनको देख कर अन्दर-ही-अन्दर प्रसन्न होता रहता है कि इन्द्रियों को उनकी रुचि की वस्तु मिल गयी है। किन्तु फिर भी यहाँ मन की इन्द्रियों से कुछ अंशों में एकता रहती है। मन ही इन्द्रियों को आनन्दोपभोग हेतु शक्ति प्रदान करता है। यदि मन इन्द्रियों से अपनी शक्ति खींच ले, तो वे शान्त हो जायेंगी और मृत हो जायेंगी। सुखदायक तथा कष्टप्रद, दोनों ही प्रकार के अनुभव शक्ति का ह्रास करते हैं; क्योंकि मन का बहाव बाहर की ओर होता है। इसलिए दिन के अनुभव सुखप्रद या कष्टप्रद कैसे भी हों, मन थका हुआ अनुभव करता है। वह निद्रा की अभिलाषा रखता है और नींद के सच्चे और शुद्ध आनन्द का उपभोग करना चाहता है।
याद रखें। जब आप स्वयं को थका हुआ और शक्तिहीन अनुभव करते हैं, उस समय निद्रा की अनिवार्य आकांक्षा यह दर्शाती है कि सच्चा सुख और सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। यदि इन्द्रिय-सुख आपको सच्चा सुख प्रदान करते, तो मात्र एक गहरी नींद के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ने लिए तैयार न हो जाते। जब नींद आप पर आधिपत्य कर लेती है या अन्य शब्दों में इन्द्रियाँ और मन थके हुए हों, तो सबसे स्वादिष्ट व्यंजन भी आपको नहीं ललचाता, सबसे सुन्दर दृश्य भी आपको नहीं लुभाता, सबसे मधुर संगीत आपको उबाऊ लगता है, सुगन्ध का भी अनुभव नहीं होता है। और पत्थरों की शय्या महँगे नर्म बिस्तर का सुख देती है। यदि सुख इनमें ही होता, तो आप इन्हीं में लगे रहते, इन्हें छोड़ कर सुख को स्वयं के भीतर न खोजते ।
यदि आप जागते हुए गहरी नींद में चले जायें, यदि आप बाह्य जगत् के लिए पूर्ण मृत होते हुए आन्तरिक रूप से पूर्ण चैतन्य रहें, तो आप सर्वोच्च चेतना की स्थिति, निर्विकल्प समाधि का आनन्द उठा सकते हैं। इसके द्वारा जो ज्ञान, जो शक्ति, जो आनन्द आप प्राप्त करेंगे, वह अवर्णनीय होगा। निद्रा इस परमावस्था का संकेत मात्र है, और कुछ नहीं ।
सम्पूर्ण जगत् में ऐसे अरबों मनुष्य हैं, जो रात में चैन की नींद नहीं सो पाते, जो प्रगाढ़ निद्रा का आनन्द नहीं ले पाते। वे इस पृथ्वी पर कष्टमय जीवन जी रहे हैं। वे अनिद्रा के कारण विभिन्न रोगों और नाड़ी-दोषों का शिकार हैं। उनके लिए इस पुस्तक में विभिन्न उपाय सुझाये गये हैं। उनके लिए मैंने इस पुस्तक में बहुत से उपचार प्रस्तावित किये हैं। सामान्य रूप से प्राकृतिक और नामोपचार पद्धति ली गयी है। यदि रोगी कुछ अन्य प्रकार की उपचार पद्धति का प्रयोग भी करता है, तो इस मिश्र-पद्धति द्वारा रोग में शीघ्र सुधार परिलक्षित होगा।
मैं आपसे यह स्मरण रखने के लिए कहता हूँ कि आप नींद हेतु पुराने अनुभव के साथ बिस्तर पर न जायें। निद्रा आपके पास स्वयं ही आयेगी, आपको मात्र उसे निमन्त्रण भेजना है और निद्रा के स्वागत हेतु तैयार रहना है। आपको स्वयं में और अपने चारों ओर ऐसी स्थितियाँ निर्मित करनी हैं, जिससे नींद आपके पास आने के लिए ललचाये। बस, इतना ही, और कुछ नहीं करना है तथा जब तक नींद न आये, उसकी प्रतीक्षा करनी है।
यह इसलिए क्योंकि एक साधक जो सतत समाधि में अवस्थित रहता है, उसके सिवा अन्य कोई नहीं जानता कि वह निद्रा में कब जाता है या अन्य शब्दों में निद्रा किस द्वार से प्रवेश करती है, चाहे वह जागा हो या सोया हो अथवा स्वप्न देख रहा हो (क्योंकि स्वप्न भी जाग्रत अवस्था का विस्तार ही है)। क्योंकि जब आप सोने वाले होते हैं, उसी समय वह ज्योति जिसकी सहायता से आप जानते, काम करते और विचार करते हैं, आपके हृदय में आने वाली रहस्यमय अतिथि - निद्रा द्वारा बुझा दी जाती है।
यहाँ पुनः आप निद्रा और समाधि में गहरी समानता पायेंगे। आपआत्मा के प्रकाश में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक आपका अस्तित्व है, प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। प्रकाश के अनुभव के पूर्व अहंकार समाप्त होना चाहिए। ईश्वर आपके सामने स्वयं ही प्रकट होंगे। आप उनसे आने के लिए भावपूर्ण प्रार्थना मात्र कर सकते हैं। आप नहीं जान सकते, वे कैसे आयेंगे, कब आयेंगे और किस द्वार से आयेंगे। आपको सभी द्वार खुले रखने होंगे। आपको अपना अन्तःकरण स्वच्छ, शुद्ध और क्षिपग्राही रखना होगा। जब वे प्रवेश करेंगे, वे तत्क्षण आपकी बुद्धि की भ्रामक ज्योति, जिसके द्वारा आप इस दृश्यमान जगत् को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, बुझा देंगे। उनके स्नेहपूर्ण हाथों में आप स्वयं को, स्वयं के अस्तित्व को भूल जायेंगे। जब तक आप विषय-वस्तुओं को जानते हैं, उन्हें नहीं जान सकते। आपको उनका अनुभव एक रहस्यमय तरीके से होगा—जैसा किआप गहन निद्रा में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, यह ठीक वैसा ही होगा। वह तुच्छ साधन जिससे आप अपनी जाग्रतावस्था के अनुभव का अन्वेषण करते हैं, जिससे आप विषयों को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते और उनका आनन्द उठाते हैं, वह बुद्धि दोनों ही अवस्थाओं में अनुपस्थित रहती है। इसलिए आप नींद अथवा समाधि में कैसे जाते हैं, इसका आपको ज्ञान नहीं होता। दोनों ही विषयों में आप मात्र निमन्त्रण भेजें और स्वयं को तैयार रखें।
सबसे श्रेष्ठ निमन्त्रण आत्म-समर्पण है, दिव्यता के प्रति सम्पूर्ण और स्वतन्त्र आत्म-समर्पण जो आपको समाधि में अत्यन्त शीघ्र प्रवेश हेतु, तत्काल भाव समाधि का आनन्द उठाने के लिए और सदैव सहज अवस्था में रहने के योग्य बनायेगा ।
पुनः यह आत्म-समर्पण अनिद्रा के लिए एकमात्र त्रैलोक्य- चिन्तामणि है।
आप सब पूर्ण आत्म-समर्पण और आत्मा पर ध्यान द्वारा जाग्रत निद्रा या समाधि का उपभोग करें! आप सभी इसी जन्म में जीवन्मुक्ति के सुख का उपभोग करें!
स्वामी शिवानन्द
२४ मार्च, १९५१
परमानन्द-प्राप्ति के मार्ग
१. ईश्वर अज्ञानता, दुःख और भय को दूर करने वाले हैं। वे अनन्त सुख के दाता हैं। उन्हें जानें। वे आपके
भीतर सदा निवास करते हैं।
२. ईश्वर में पूर्ण आस्था रखें। आस्था और विश्वास ही ईश्वर का द्वार है। आस्था चमत्कार कर सकती है।
३. अपने छोटे-से-छोटे कार्य में अपने हृदय, मन, बुद्धि और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का
रहस्य है।
४. आहार, पीने, शयन, मनोरंजन और सभी बातों में संयम रखें।
५. जीवन के उचित नियमों का पालन करें। स्वास्थ्य, शक्ति, सफलता और ईश्वर - साक्षात्कार के लिए
प्रयत्न करें।
६. मुक्त - हस्त से दान करें। सब कुछ दान करें। यही प्रचुरता का रहस्य है।
७. सदैव विश्वास और दृढ़ संकल्प से काम करें। अपने संकल्प में दृढ़ रहें और अपने निर्णय में अटल रहें।
लौह-संकल्प रखें।
८. अतीत को जाने दें। अतीत पर मिट्टी डालें। आपके लिए देदीप्यमान भविष्य सामने है। प्रयत्न, प्रयत्न,
प्रयत्न करें।
९. सदा प्रसन्न रहें और चिन्ताओं को मुस्करा कर दूर कर दें। इच्छाओं, स्वार्थ और घृणा को निकाल कर
अपनी संकल्प-शक्ति का विकास करें।
१०. विषय-भोगों में लिप्तता आपको नाश की ओर ले जायेगी। वैराग्य आपको अमरत्व की ओर अग्रसर
करेगा। राग और आसक्ति छोड़ें।
११. उचित विचार सही चेष्टा, अच्छे कर्म और एक प्रशंसनीय चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए सही
विचारों का विकास करें।
१२. शुद्ध विवेक-बुद्धि रखें। स्वयं को स्वार्थ से मुक्त करें। मैं और मेरे पन की भावना को नष्ट करें। मोक्ष
प्राप्त करें। मुक्त हो जायें। परमानन्द का लाभ उठायें।
१३. सेवा करें, प्रेम करें, दान करें और इन्द्रियों तथा मन को संयमित करें। भले बनें। भला करें। दयालु बनें।
पवित्र बनें। धैर्यवान् बनें।
१४. आगे बढ़ें। विकास करें। उन्नति करें। अलगाव की भावना को नष्ट करें। सबके साथ घुलें मिलें और
दिव्य प्रेम का विकास करें। निःस्वार्थ बनें।
१५. सावधान और परिश्रमी बनें। ध्यान दें और प्रार्थना करें। उपवास और ध्यान करें। अनुभव करें। भय,
चिन्ता और व्याकुलता को मन से हटा दें।
१६. साधुओं की सेवा करें। सत्संग में जायें। भगवान् का नाम गायें। एक महीने एकान्तवास करें। फल और
दूध पर रहें। ध्यान करें।
१७. मैं कौन हूँ? संसार क्या है ? ब्रह्म क्या है ? बन्धन क्या है? मुक्ति क्या है? माया क्या है? अविद्या
क्या है? विचार करें।
१८. विरागी बनें। मन को शान्त करें। मन को सदा एक बिन्दु पर केन्द्रित तथा सम स्थिति में रखें।
१९. आध्यात्मिकता को स्वीकारें। पवित्रता का अभ्यास करें। श्रेष्ठता का विकास करें। समाज-सेवा करें।
दानशीलता का अभ्यास करें। दिव्यता प्राप्त करें।
२०. शुद्धता रखें। ध्यान करें। मनन करें। चित्त को एकाग्र करें। सिद्धि प्राप्त करें।
विषय-सूची
उत्तर दिशा की ओर सिर करके न सोयें
इच्छा-शक्ति निद्रा प्राप्त करना
अनिद्रा रोग के लिए होमियोपैथिक औषधियाँ
नीचे बताये उपायों को करें : आप अच्छी नीद सोयेंगे
हृदय को झंकृत करने वाले कीर्तन
|
अच्छी नींद कैसे सोयें
|
आत्म-समर्पण का गीत
सोने जाने से पूर्व इस पवित्र मन्त्र को पन्दरह मिनट तक गायें। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करें। आपका मन सत्त्व से परिपूर्ण हो जायेगा और आप गहरी निद्रा का आनन्द उठायेंगे।
(धुन: सुनाजा सुनाजा)
दीनबन्धु दीनानाथ विश्वनाथ हे विभो;
पाहिमान् त्राहिमाम् प्राणनाथ हे प्रभो ।
"हे विश्व के स्वामी! हे सर्वव्यापक आत्मा! आप दीनबन्धु हैं, आप निर्बलों के, निर्धनों के, पतितों के रक्षक हैं। हे मेरे जीवन के स्वामी! हे मेरे जीवन के पालनहार ! मेरी रक्षा करो! मुझे बचाओ!"
यह सर्वाधिक प्रबल सूत्र है जो आपका तत्क्षण आत्मोत्थान करेगा ।। आपको सुख और शान्ति देगा। यह आपको शक्ति और ऊर्जा प्रदान यह करेगा। यह सन्देह और निराशा को दूर ले जायेगा। यह दुःख और भ्रम को बाहर निकाल देता है। यह उस भेद-बुद्धि को नष्ट कर देता है जो आपको ईश्वर से दूर रखती है। यह आपको संसार से बाँधने वाले कर्तृत्व-भोक्तृत्व अभिमान को नष्ट कर देता है। यह आपको ईश्वर के समक्ष निरहंकार और नम्र बनायेगा। यह आपके अहंकार को चूर-चूर करके नष्ट कर देगा। यह आपको अन्तर्मन से ईश्वर का ज्ञान कराने में सहायक होगा और आपके हृदय को विशाल बनायेगा ।
जब आप इसे दोहरायेंगे, आप तत्क्षण अनुभव करेंगे कि 'ईश्वर ही सब कुछ हैं, मैं कुछ नहीं हैं। आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है। आप उनके विराट्स्वरूप के दर्शन का आनन्द उठायेंगे। मात्र इतना ही नहीं, आप अनुभव करेंगे कि वह आपके जीवन के स्वामी, अवलम्ब, स्रोत और लक्ष्य भी हैं। वे सर्वव्यापक और आपके हृदय के भीतर निवास करने वाले स्वामी हैं। वे आपकी श्वास से भी अधिक पास हैं। वे आपके जीवन को धारण करते हैं। वे आपको विचार करने, बोलने और कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी ही शक्ति से आप उनसे प्रार्थना करने के योग्य, उनकी पूजा करने के योग्य और यहाँ रहने के योग्य होते हैं। मन को इस प्रकार बना कर आप उनसे प्रार्थना कीजिए- "मैं आपका हूँ, सब आपका है, मेरे प्रभु मुझे बचायें, मेरी रक्षा करें।" आप उनसे रोगों से बचाव या गरीबी दूर करने हेतु प्रार्थना न करें। आप उनसे इस भवसागर से बचाने हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। आप उनसे माया की बेड़ियों से बचाने हेतु कह सकते हैं। आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए— "मुझमें से मेरे-पन की भावना को नष्ट कर मेरी रक्षा करें।” या अन्य शब्दों में आपको स्वयं को प्रभु में समाहित करने की उत्कण्ठा रखनी चाहिए और उनसे अपने अहंकार से स्वयं को बचाने की भिक्षा माँगनी चाहिए।
जिस क्षण आप इस प्रार्थना को सम्पूर्ण हृदय और आत्मा से करेंगे, ईश्वर उसी समय आपके पास दौड़े चले आयेंगे; वे तुरन्त आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे।
आप ऐसे भी गा सकते हैं:
पाहिमाम् पालयमाम्, पाहिमाम् रक्षमाम् ।
पाहिमाम् पाहिमाम्, त्राहिमाम् त्राहिमाम् ।।
निद्रा की कविता
हे निद्रा, हे प्यारी निद्रा !
हे निद्रा शक्ति,
तुम प्रकृति की मृदु परिचारिका हो।
पौष्टिक, मृदुल और स्फूर्तिदायक हो ।
हताशा, दुःख और दर्द में
तुम शान्त करने वाला लेप और बलवर्धक औषधि हो ।
मुझे ब्रह्म तक ले कर जाओ और परमानन्द में स्नान कराओ।
मेरी नाड़ियों और मस्तिष्क को आरोग्य प्रदान करो।
और उन्हें ऊर्जा से परिपूर्ण करो।
उस देवी को जो निद्रा का रूप है, मेरे विनम्र प्रणाम |
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यैः नमो नमः ॥
निद्रा क्या है ?
अभाव-प्रत्यय-आलम्बन--वृत्ति निद्रा ।।
अभाव की प्रतीति को आश्रय करने वाली वृत्ति निद्रा है (योगसूत्र-समाधिपाद, १०) ।
जब तमोगुण की प्रबलता होती है तथा सत्त्वगुण और रजोगुण शान्त होते हैं, बाह्य जगत् का कोई ज्ञान नहीं होता, तब निद्रा प्रकट होती है। कुछ लोगों का सोचना है कि निद्रा में वृत्ति-शून्यता होती है; लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय भी आपके भीतर स्मरण-शक्ति होती है, तभी तो आप जागने पर कहते हैं— “मैं बहुत गहरी नींद सोया; मुझे कुछ नहीं पता।" नींद के समय मन में एक विशेष वृत्ति (अभाव रूप वृत्ति) होती है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि निद्रा मन की वृत्ति का रूपान्तरण नहीं है। यदि ऐसा होता, तो नींद से जागने पर आपको यह याद नहीं रह सकता कि 'मैं गहरी नींद सोया।' जो आपने अनुभव ही नहीं किया, वह आपको कदापि स्मरण नहीं रह सकता। निद्रा एक विशेष प्रकार की वृत्ति है। यदि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो अन्य वृत्तियों की तरह इसे भी नियन्त्रित करना होगा।
निद्रा का तत्त्व-ज्ञान
उस सच्चिदानन्दब्रह्म को प्रणाम जो तीनों अवस्थाओं—जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति का मूक साक्षी है। निद्रा श्रेष्ठ आयुर्वर्धक रसायन और बलवर्धक औषधि है। निद्रा क्लान्त मनुष्य को विश्रान्ति प्रदान करने वाली प्राकृतिक औषधि है। निद्रा वह स्थिति है जिसमें मन कारण शरीर में शान्ति से विश्राम करता है। मन इसके कारण में विलीन हो जाता है। वृत्तियाँ और वासनाएँ सुप्त या सूक्ष्म हो जाती हैं और मन के सभी कार्यों को रोक देती हैं। भटकता हुआ मन विश्राम प्राप्त करता है। यह मन को उसके स्रोत में विश्राम दे कर उसे नयी ऊर्जा और शान्ति प्रदान करने का प्रकृति का तरीका है। निद्रा में मन का उसके मूल में अस्थाई अवशोषण या मनोलय होता है।
नींद में गहन तम होता है। तम सत्त्व और रज को पराजित कर देता है। उदान वायु जीव को जाग्रत अवस्था से आनन्दमय कोष या कारण शरीर में ले जा कर विश्राम कराती है।
अच्छी गहरी नींद के बाद व्यक्ति पूर्णतया प्रसन्न या विश्रान्त अनुभव करता है। निद्रा एक तामसिक अवस्था है; क्योंकि इसमें न तो क्रियाशीलता होती है, न ही जागरूकता। सोया हुआ मनुष्य बाह्य जगत् के प्रति अचेतन होता है। वह अपने भौतिक शरीर के प्रति भी चैतन्य नहीं रहता। उसे यह भी चेतना नहीं रहती कि वह सोया है।
किन्तु निद्रा किसी पत्थर या लकड़ी के लट्टे की तरह की तामसिक अवस्था नहीं होती। मन और शरीर में निद्रा की अवधि में परिवर्तन होते हैं। नींद में शरीर और मन तथा नाड़ियाँ जीवन-शक्ति से परिपूर्ण हो जाती हैं, उनकी मरम्मत होती है जिससे वे नये कार्य हेतु तैयार हो जाती है। नींद में मनुष्य सुख, प्रसन्नता और समस्त कष्टों से मुक्ति का अनुभव करता है। इसलिए नींद शरीर और मन को स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक है।
अच्छी नींद के बिना कोई भी पूर्ण स्वास्थ्य का उपभोग नहीं कर सकता। नींद मस्तिष्क और नाड़ियों को विश्रान्ति तथा स्वास्थ्य प्रदान करती है। निद्रा एक ऐसा मल्हम है जो थकी हुई नाड़ियों को आराम पहुँचाता है। यह शरीर, मन और नाड़ियों को ऊर्जा तथा जीवन से परिपूर्ण करती है।
मन और शरीर एक समयान्तराल के उपरान्त या भौतिक मस्तिष्क और मानसिक शरीर के द्वारा किये गये कार्यों की प्रत्येक श्रेणी के पश्चात् विश्राम चाहते हैं।
रोगी मनुष्य अस्वस्थता के कारण सो नहीं पाता ; किन्तु यदि उसे नींद आ जाये, तो उसे अधिक आराम का अनुभव होगा। वह अपना कष्ट भूल जायेगा। नींद के समय सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नींद में कमी से रोग की तीव्रता अधिक हो जाती है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि नींद न आने के कारण रोग और अधिक गम्भीर हो गया है। और वैसे भी नींद न आना स्वयं ही एक रोग है; इसलिए नींद अनिवार्य है।
मन को जैसे-जैसे आवश्यक विश्राम दिया जाता है, वह जाग्रत अवस्था के संस्कारों के द्वारा बलपूर्वक विषय-वस्तुओं की ओर ले जाया जाता है।
यह कामना या रजोगुण का बल है जो मनुष्य को नींद से वापस जाग्रत चेतना में लाता है। जिस प्रकार एक स्प्रिंग जो हाथ से दबा कर रखी हुई हो, से जब दबाव हटा लिया जाता है, तो वह पुनः अपनी वास्तविक लम्बाई और आकार को ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार गहरी नींद आ जाने के बाद दबे हुए विचार और अभिलाषाएँ मुक्त हो जाती हैं और मनुष्य पुनः जाग्रत चेतना को प्राप्त कर लेता है।
वास्तविक रूप से जाग्रत चेतना में आने के पूर्व मनुष्य अर्ध-चेतनावस्था में आता है जहाँ वह न तो जाग्रत रहता है, न स्वप्न देखता है। रात के समय बहुत समय तक मनुष्य तन्द्रा और आलस्य में रहता है। स्वप्न भी नींद में विघ्न डालते हैं। यही कारण है कि मनुष्य की सम्पूर्ण सन्तुष्टि के साथ अच्छी और गहन निद्रा का समय अत्यन्त थोड़ा होता है। छह घण्टे की नींद जो स्वप्न, आलस्य और तन्द्रा से बाधित हो, उसके स्थान पर एक घण्टे की गहन निद्रा मनुष्य को अधिक विश्रान्ति प्रदान करती है।
नींद के समय में भोजन की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। एक पेटू मनुष्य निद्रालुता का अनुभव करता है। वह आठ बजे तक शय्या छोड़ना पसन्द नहीं करता। वह आलस्य से परिपूर्ण रहता है। एक मिताहारी मनुष्य शीघ्र ही शय्या त्याग देता है। वह थोड़ी किन्तु गहरी नींद से सन्तुष्ट रहता है।
पशु भी सोते हैं। विभिन्न पशुओं में निद्रा की अवधि भिन्न-भिन्न होती है। कुत्ते बहुत कम सोते हैं। वे बाधित निद्रा का अनुभव करते हैं। मछलियाँ बिलकुल नहीं सोतीं ।
गहन और स्वप्नों से रहित निद्रा हेतु मानसिक शान्ति, चिन्ता, भय, व्याकुल बना लेना और जीवन में उत्तरदायित्वों की अनुपस्थिति और रोगों से मुक्ति — ये सभी सहायक हैं। जो शिथिलीकरण क्रिया को जानता है, उसे बिस्तर में लेटने के साथ ही तुरन्त गहरी नींद आ जाती है। रात के समय हलका भोजन लें। दूध और फल । रात को चावल न खायें। प्राणायाम का अभ्यास करें। आप अपनी नींद को कम कर सकेंगे और आपके स्वास्थ्य पर भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यदि आप गहरी नींद सो पायें, तो आप नींद की समयावधि को कम करके उस समय का उपयोग अन्य उपयोगी कार्यों में कर सकते हैं। यदि आप गहरी नींद का समय घटा सकें, तो आप अपनी साधना में अधिक समय दे सकते हैं। यदि आप दो घण्टे की नींद कम कर सकें, तो आप इस समय का सदुपयोग जप और ध्यान में कर सकते हैं। आठ-दस घण्टे की स्वप्नों से पूर्ण निद्रा से छह घण्टों की गहन निद्रा अधिक श्रेष्ठ है।
ऐसे लोग हैं जिन्होंने नींद पर विजय पायी, उन्हें गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन और लक्ष्मण गुडाकेश थे। नेपोलियन बोनापार्ट का नींद पर आधिपत्य था । वह युद्धभूमि में भी अच्छी नींद सोने का आदी था। वह एकदम निश्चित समय तक सो सकता था। पाँच या दस मिनट की गहन निद्रा उसे अगले कार्य के लिए उत्साह से भर देती थी।
महात्मा गान्धी का भी नींद पर पूर्ण नियन्त्रण था। उन्हें श्रेष्ठ, गहन और स्वप्नों से रहित निद्रा प्राप्त थी। वे बहुत थोड़े-से समय के लिए सोते थे और एक निश्चित समय पर जग जाते थे और अपने दैनिक कार्यों को करने लग जाते थे
ऑफिस में काम करने वाले बाबू की तुलना में एक किसान या परिश्रमी मजदूर अधिक गहरी नींद सोता है; क्योंकि कठिन श्रम के कारण शरीर और मन थक जाते हैं, जब कि प्रथम विषय में ऐसा नहीं होता। शारीरिक थकावट से मानसिक थकान भी हो जाती है। शारीरिक श्रम कम और मानसिक श्रम अधिक करने वाले व्यक्तियों को नींद कम आती है। कुछ लोगों में शरीर की तुलना में मन कम थकता है। सारे दिन काम करने वाले कुली को अधिक नींद की आवश्यकता होती है। वह गहरी नींद सोता है। जब आप सपने देखते हैं, मन को विश्राम नहीं मिलता। मन जाग्रत अवस्था के अनुभवों के काल्पनिक प्रतिरूपों से खेलता रहता है। इसलिए यदि आप नींद में पूरा आराम चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप सपनों से मुक्ति पा लें। यदि आप सपनों से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने मन की चिन्ताओं, व्यग्रताओं तथा आकुलताओं से मुक्त और ईश्वर भक्ति एवं वैराग्य से परिपूर्ण रखना होगा।
जब मन व्यर्थ के विचारों में लगा रहता है, तो शीघ्र नहीं थकता । यह हवाई महल बनाता रहता है। एकाग्र मन शीघ्र ही थक जाता है। कठिन परिश्रम करने से शरीर शीघ्र ही थक जाता है। मन निद्रा में मुख्य कारक है। निद्रा शरीर और मन दोनों के लिए होती है। यदि शरीर थका हो और मन सोना नहीं चाहता हो, तो नींद नहीं आयेगी।
जब हम सोने जाते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे शरीर पर यह प्रभाव होता है। कि हमें लेटना पड़ता है। उसके बाद हम आँखें बन्द करते हैं। जब हमारे ऊपर नींद का आधिपत्य हो जाता है, तो आवाजें अदृश्य हो जाती हैं, मन अन्तर्मुखी हो जाता है। प्रथम अवस्था में हम आवाजों को सुनते और बातों को समझते हैं। बाद में आवाजें तो सुनायी देती हैं, किन्तु हम उनके तात्पर्य को ग्रहण नहीं कर पाते। फिर धीरे-धीरे ध्वनियाँ भी समाप्त हो जाती हैं और हम बाह्य जगत् और शरीर की चेतना से परे चले जाते हैं। इसी क्रम से मन पहले अर्ध-चेतनावस्था में आता है, फिर उसके बाद जाग्रत अवस्था में। आकाश से वायु जन्म लेती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से जीवन और स्वास्थ्य। गहन निद्रा में इन्द्रियों के लय तथा पुनः जाग्रत अवस्था में आने के लिए भी यही क्रम रहता है।
जब तक मन शरीर के आराम पर केन्द्रित रहता है, नींद नहीं आती। अस्वस्थ मनुष्य को नींद न आने का यही कारण है। रोग उसके मन को शरीर के विषय में अधिक सोचने के लिए विवश करता है। उसे शरीर के दर्द की जितनी अधिक चेतना होगी, नींद उतनी कम होगी; किन्तु उन रोगों में जिनमें दर्द समयान्तराल से या रुक-रुक कर होता है, रोगी बीच-बीच में सोता रहता है।
निद्रा का विश्लेषण चेतना के पूर्ण अभाव तथा पूर्ण शिथिलीकरण द्वारा किया जा सकता है। जब मनुष्य सोता है, तो शरीर और मन दोनों पूर्ण विश्राम करते हैं। मन हृदय की हिता नाड़ी में विश्राम करता है और आत्मिक आनन्द का उपभोग करता है। विभिन्न क्रियाविधियों में व्यय होने वाली ऊर्जा की निद्रा में क्षति पूर्ति हो जाती है। इसलिए नींद लेना बहुत आवश्यक है। बिना नींद के नाड़ियाँ कमजोर हो जायेंगी, विभिन्न अंग क्षीण हो जायेंगे और शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा ।
निद्रा रात्रि के समय अधिक विश्रान्ति प्रदान करती है; क्योंकि तब बाधा डालने वाली आवाजें नहीं होतीं। मन भी दिन के श्रम के कारण थका रहता है। रात प्राकृतिक रूप से सोने का समय है। दिन काम के लिए बना है। जब हम प्रकति के नियमों के अनुरूप चलते हैं, तो हम स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के भयंकर हानिकर परिणाम होते हैं।
युवा मनुष्य की तुलना में बच्चा अधिक समय तक सोता है। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, नींद कम हो जाती है। यह शारीरिक अंगों की अक्षमता के कारण होता है।
जब बैठी हुई अवस्था में नींद आप पर आधिपत्य कर लेती है, तो शरीर की प्रवृत्ति लेट जाने की होती है। शरीर नीचे खिसक जाता है। सिर लटक जाता है। ऐसा इसलिए होता है; क्योंकि मन काम नहीं करता। इसलिए तब पेशियों के मध्य सामंजस्य नहीं रहता। मन भौतिक शरीर से अपने सम्बन्ध तोड़ लेता है, इसलिए शरीर नीचे गिर पड़ता है।
प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से अत्यधिक प्रेम करता है। व्यक्ति निद्रा में अचेतन रहता है। निद्रा की अवधि में जीव को रेंगने वाले प्राणियों और अन्य जीव-जन्तुओं से हानि का पूर्वानुमान रहता है। इसलिए वह ऐसे स्थान की खोज करता है जहाँ वह खतरे से मुक्त रहे। उसे अच्छे वातावरण—जैसे अच्छा स्थान, नर्म बिस्तर आदि की आवश्यकता रहती है। ईश्वर की माया अत्यन्त गूढ़ है।
आप सभी जाग्रत निद्रा, तुरीयावस्था या चतुर्थ अवस्था, जो तीनों अवस्थाओं से श्रेष्ठ है, जहाँ न तो जगत् है न शरीर, न जाग्रत, न स्वप्न, न सुषुप्ति - उस निद्रा में विश्राम करें।
निद्रा की आवश्यकता
जिस प्रकार एक चिड़िया अपने भोजन की खोज में प्रातः काल से आकाश में ऊँची उड़ती है और उच्च स्थानों में इधर-उधर घूमती है एवं रात के समय अपने घोंसले में पूर्ण विश्राम करती है, उसी प्रकार जीव या जीवात्मा सारे दिन इन्द्रिय-वस्तुओं के घने वन में घूमने के बाद अपने गृह कारण शरीर में जाता है और सुषुप्ति या गहन निद्रा के आनन्द का उपभोग करता है।
मन दिन-भर कठिन परिश्रम करता है जिससे वह अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सके। वह राग और द्वेष—दोनों वृत्तियों द्वारा इधर-उधर भेजा जाता रहता है, इसलिए वह थक जाता है। प्रकृति रात के समय उसे अपनी गोद में ले कर जाती है जिससे उसकी थकी नाड़ियों और मस्तिष्क को शान्ति मिले, उसे विश्रान्ति प्राप्त हो और उसे ऊर्जा और शक्ति से सम्पन्न करती है जिससे वह अगले दिन की गतिविधि कर सके।
वेदान्तियों ने निद्रा का गहन अध्ययन करके सर्वानन्दमयी आत्मा जो सुषुप्ति अवस्था की मूक साक्षी है, उसके बारे में निष्कर्ष दिये। गहन निद्रा में मन बीज-रूप को ग्रहण कर लेता है, संस्कार और वासनाएँ सुप्त हो जाती हैं। मन जो जाग्रत अवस्था में क्रियाशील रहता है, वह सुषुम्ना नाड़ी से आत्मा में चला जाता है और विश्राम करता है। चैतन्यता या बुद्धि जो गहन निद्रा की स्थिति से जुड़ी रहती है, वह है प्रज्ञा गहन निद्रा में कारण शरीर या बीज शरीर या आनन्दमय कोष कार्य करता है, जीवात्मा के बहुत पास रहता है। अज्ञानता का पतला-सा आवरण उसे आत्मा से पृथक् करता है। जैसे-जैसे अज्ञानता का यह आवरण हटता है और वह ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और जीवात्मा आनन्द का उपभोग करता है। समस्त मनों के मूक साक्षी से मन, प्राण, इन्द्रियाँ और शरीर अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। यह आत्मा है जो वास्तव में इन्द्रियों, मन, शरीर और कार्य करने वाली प्रकृति को चलाती है। इसीलिए आत्मा सर्वकर्ता और अकर्ता, सर्वभोक्ता तथा अभोक्ता है।
निद्रा प्राकृतिक शक्तिवर्धक है जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। व्यक्ति जितनी गहरी नींद सोयेगा, वह उतना अधिक स्वस्थ होगा। थकान को दूर करने की आपकी शारीरिक और मानसिक योग्यता पर ही आपकी नींद की अवधि निर्भर करती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आप काम दक्षतापूर्वक नहीं कर सकेंगे। नींद की मात्रा आयु, स्वभाव और श्रम के ऊपर निर्भर करती है। एक पुरानी कहावत के अनुसार पुरुष के लिए ६ घण्टे, स्त्री के लिए ७ घण्टे और मूर्ख के लिए ८ घण्टे की नींद आवश्यक होती है। एक बच्चे के लिए १० घण्टे की नींद आवश्यक होती है। साठ वर्ष के वृद्ध व्यक्ति के लिए ६ घण्टे की नींद पर्याप्त है। वे प्रौढ़ व्यक्ति जो भारी कार्य करते हैं, वे आठ घण्टे सो सकते हैं। चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक आजकल निद्रा के प्रश्न पर बहुत ध्यान दे रहे हैं।
प्रत्येक के लिए ६ घण्टे की नींद पर्याप्त है। १० बजे रात को सोने जायें और ४ बजे प्रातः उठ जायें। “जल्दी सोना और जल्दी जागना मनुष्य को स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान् बनाता है।” नेपोलियन बोनापार्ट मात्र चार घण्टे की नींद में विश्वास रखता था। बहुत अधिक सोने से मनुष्य आलसी और सुस्त हो जाता है। जो आवश्यक है, वह है निद्रा का स्तर। यदि आप एक या दो घण्टे स्वप्न-रहित गहरी नींद सो लें, तो आप पूर्ण विश्रान्त हो जायेंगे । घण्टों बिस्तर में लेटे रह कर करवटें बदलते रहने से 1 कोई लाभ नहीं होगा। बहुत अधिक सोने से पूर्वकालिक क्षय और मस्तिष्क की शक्ति क्षीण होती है।
देर रात को न सोयें। जब आप सोयें, अपने सोने के कमरे की सारी खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दें। नींद समय आप जितनी अधिक प्राणवायु भीतर लेंगे, अगले दिन आप उतनी अधिक विश्रान्ति का अनुभव करेंगे। नींद लाने हेतु किसी औषधि का प्रयोग न करें। यदि आपको स्वाभाविक रूप से नींद न आती हो, शान्त मन से १५ मिनट खुली हवा में घूमने चले जायें; फिर सोने जायें। आपको निश्चय ही विश्रान्तिदायक निद्रा आयेगी।
रात्रि में पाचन अंग शान्तिपूर्वक और निर्बाध रूप से कार्य करते हैं; इसलिए रात के समय आपको हलका भोजन ग्रहण करना चाहिए, चाय या तेज काफी नहीं लेनी चाहिए। बायीं करवट लेट कर सोना चाहिए। यह आमाशय को रिक्त करने में सहायक है। इससे सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी चलने लगती है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सोने जायें। ढीले और हलके कपड़े पहनें। भारी कम्बल न ओढ़ें।
जब आप सोने जायें, अपने मन तथा शरीर को शिथिल रखें। कुछ प्रार्थना या गीता और उपनिषद् के पवित्र श्लोक पढ़ें। दस मिनट तक माला फेरें तथा ईश्वर और कुछ दिव्य गुणों का ध्यान करें। हवाई किले न बनायें। अभी योजनाएँ न बनायें, कल्पनाएँ न करें। यदि आपके मन में किसी के प्रति बुरा अनुभव या दुर्भावना है, तो उसे भूल जायें। मात्र सुखदायक और स्वच्छ विचार रखें।
सारी रात जागते रहना रात्रि जागरण कहलाता है। यदि आप वैकुण्ठ एकादशी, शिवरात्रि, गोकुल अष्टमी, भगवान् कृष्ण के जन्म-दिवस (जन्माष्टमी) पर रात्रि जागरण करेंगे, तो आपको अगणित लाभ होंगे। आप प्रत्येक एकादशी पर भी जागरण कर सकते हैं। पूर्णोपवास निद्रा के नियन्त्रण में भी सहायक हैं। निद्रा के नियन्त्रण हेतु चाय आवश्यक नहीं है। यदि आप बाह्य औषधि पर निर्भर रहेंगे, तो आप आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
आपका आधा जीवन निद्रा में व्यर्थ नष्ट हो जाता है । वे आध्यात्मिक साधक जो कठोर साधना करना चाहते हैं, उन्हें अपनी निद्रा की अवधि में धीरे-धीरे कमी करनी चाहिए। वे ध्यान के द्वारा यथार्थ विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम तीन माह तक उन्हें अपनी नींद की अवधि आधा घण्टे कम करनी चाहिए। रात को १०.३० बजे सोने के लिए जायें और प्रातः चार बजे उठें। ४ घण्टे की नींद पर्याप्त है। आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। एक समय के बाद आप अर्जुन और लक्ष्मण की भाँति गुडाकेश (नींद को जीतने वाले) बन जायेंगे और योगियों की भाँति सर्वानन्दमयी, जाग्रत निद्रा निर्विकल्प समाधि में विश्राम करेंगे।
निद्रा में जीव
जीवात्मा या कूटस्थ ब्रह्म का चिन्तन और मन का चिन्तन —दोनों ही अभिन्न रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं। मानव-प्राणी में मन की वृत्तियों के निर्माण के बाद उसे जीवात्मा नाम दिया गया है। वृत्तियों के निर्माण के पूर्व कोई जीव नहीं होता। मन वृत्तियों से ढका, घिरा हुआ और पूरित है। वासना के बल से जीव और मन इन्द्रिय-विषयों में घूमता रहता है। बिना मन के कोई जीव नहीं होता।
निद्रा में जीव मन के साथ प्रकृति अथवा कारण शरीर में विश्राम करता है। विक्षेप-शक्ति जो कि बहुत से मानसिक उद्वेलनों का कारण है. वह निद्रा की अवधि में जीव के भीतर कार्य नहीं करती। किन्तु मन अभी भी आवरण या अज्ञानता से ढका रहता है। वह शान्त रहता है; क्योंकि तब विक्षेप-बल का अभाव रहता है, इस समय उसे इधर-उधर नहीं घसीटा जाता। कारण शरीर ही आनन्दमय कोष है। इस कारण जीव निद्रा में आनन्द का उपभोग करता है। वह आनन्दमय पुरुष है। वह प्रज्ञा है। यह एक प्रकार का दृष्टिकोण है।
नींद के समय मन अन्य विषयों पर विचार नहीं करता। मन पहले हृदय नाड़ी में, फिर हृदयावरण में, फिर आन्तरिक हृदय में प्रवेश करके अन्त में मुख्य प्राण में विश्राम करता है। जीवात्मा हृदयाकाश में प्रवेश करके कूटस्थ ब्रह्म में विश्राम करता है। वह स्वयं ब्रह्म में, आनन्द में लीन हो जाता है। वह ब्रह्म में अपने सच्चिदानन्दस्वरूप में डुबकी लगा कर उसी प्रकार आनन्दित होता है जैसे तीर्थयात्री पवित्र प्रयाग में डुबकी लगा कर प्रसन्न होते हैं। यह दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण है।
यह एक सामान्य प्रश्न है कि सोते समय कौन-सा सिद्धान्त कार्य करता है जो आत्मा या जाग्रत जीव में इसका स्मरण छोड़ देता है कि उसने गहरी नींद का आनन्द उठाया। इसका सादा-सा उत्तर यह है कि यह वह अज्ञात आत्मा है जिसे कूटस्थ कहते हैं।
यह विरोध इस आधार पर किया जा सकता है कि वहाँ परस्पर मिथ्या धर्म (परस्पर अध्यास) होता है। कूटस्थ जो जीव के साथ अवर्णनीय रूप से मिश्रित है, फिर भी उससे भिन्न है, वह जीव की आन्तरिक आत्मा है और इसी कारण जीवात्मा जो स्रष्टा के साथ एक होना चाहता है, उसके अनुभव जीव को स्मरण रखने हेतु प्रेरित करते हैं।
यहाँ भी विरोध हो सकता है कि जीवात्मा अथवा कूटस्थ द्वारा निद्रा के आनन्द का स्मरण जीव के निद्रा के आनन्द की स्मृति का कारण नहीं हो सकता। इसमें यह कहना ज्यादा न्यायोचित होगा कि यह स्मरण उस साक्षी के कारण रहता है जो कि जाग्रत, स्वप्न और निद्रा तीनों में उपस्थित रहता है।
जैसे ही आप नींद से जागते हैं, आप कहते हैं— 'मैं पिछली रात बहुत अच्छी नींद सोया, मैंने इसका हृदय से आनन्द उठाया वहाँ बड़ी ठण्ढी हवा थी।' यहाँ कौन-सा सिद्धान्त है जो कह रहा है कि मुझे अच्छी नींद आयी ? और इसका दूसरा कौन-सा सिद्धान्त है जो कहता है कि 'मैं कुछ नहीं जानता।' एक ही विचारधारा के लोगों का उत्तर होगा –“अविद्या वृत्ति कहती है, मैं कुछ नहीं जानता।” शारीरिक उपनिषद् के अनुसार, "जाग्रति वह स्थिति हैं जिसमें चौदह अंग कार्य करते हैं—पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और चार आन्तरिक अंग । स्वप्न वह स्थिति है जो चारों आन्तरिक अंगों से सम्बद्ध है । सुषुप्ति वह स्थिति है जहाँ मात्र चित्त ही अंग होता है। तुरीयावस्था वह स्थिति है, जहाँ मात्र जीव होता है।" यह इस सिद्धान्त की सूक्ष्म क्रियाविधि है जिससे कि गहन निद्रा में सभी संस्कार भी सुप्त हो जाते हैं। इसलिए चित्त ही वह मूल है जो गहन निद्रा के आनन्द का स्मरण रखता है। गहन निद्रा के सुखों की स्मृति ज्ञान का श्रेय मूल तत्त्व चित्त को जाता है जो गहन निद्रा में सदा कार्य करता है। यह तीसरा दृष्टिकोण हुआ ।
स्वास्थ्य हेतु निद्रा
निद्रा का अर्थ है समस्त अंगों द्वारा विश्राम । निद्रा प्रकृति का स्वास्थ्यवर्धक कारक है। यह थके हुए मस्तिष्क, नाड़ियों और शरीर को प्रचुर ऊर्जा और विश्राम प्रदान करती है। निद्रा नाड़ी -बल का नवीन संग्रह करके नष्ट हुई कोशिकाओं की पुनः क्षति पूर्ति करती है। नींद स्वयं ऊर्जा का निर्माण करने वाली है तथा शक्ति जन्म देती है। जब आप सोये होते. हैं, तब भी आपका मूल तत्त्व सदा जाग्रत रहता है। वह तीनों अवस्थाओं जाग्रत, स्वप्न और गहन निद्रा का मूक साक्षी है। वह प्रत्येक वस्तु का स्रोत, कारण, आश्रय और अवलम्ब है। वह देवताओं का स्वामी है। वह सबकी आत्मा है। मन निद्रा में उसमें विश्राम करके शक्ति, नवीन ऊर्जा और शान्ति प्राप्त करता है।
काम के समय चाहे पैर विश्राम कर रहे हों, नाड़ियों को काम करना होता है। उन्हें इस कारण शिथिलीकरण की आवश्यकता होती है। शिथिलीकरण स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है। नींद हमें यह शिथिलीकरण प्रदान करती है। नींद से पूर्ण शिथिलीकरण होता है।
नवजात शिशु सोता ही रहता है। कुछ दिनों तक बच्चा दिन में मात्र दो घण्टे ही जागता है। पाँच वर्ष की आयु तक बच्चा ८ से १० घण्टे तक सोता है। एक पूर्ण वयस्क पुरुष को ६ घण्टे की नींद की आवश्यकता होती है। स्त्री के लिए ७ घण्टे की नींद पर्याप्त है। किशोर वय के बच्चे के लिए ७ से ८ घण्टे की नींद पर्याप्त रहती है। नींद में स्वप्न दिखायी दें या नींद बाधित हो, तो पूर्ण शिथिलीकरण नहीं प्राप्त होता । चालीस वर्ष की आयु के पश्चात् नींद कम हो जाती है।
ऐसे कई मनुष्यों के उदाहरण हैं जो बहुत कम सोने के बाद भी उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ और फुर्तीले हैं जो अधिक सोते हैं। स्केलिज़र जो एक महान् फ्रेंच विद्वान् थे तथा शेक्सपियर के समकालीन थे, तीन घण्टे सोते थे। वेलिंग्टन और सर हेनरी थॉम्पसन प्रसिद्ध चिकित्सक थे और अस्सी वर्ष की आयु तक जीवित रहे। दोनों ने ही यह जाना कि चार घण्टे की नींद पर्याप्त होती है। इसी प्रकार एडीसन भी ३० तक तीन घण्टे ही सोते थे।
नींद विश्राम हेतु आवश्यक है; अतः इसके लिए कड़े नियमों से नहीं चला जा सकता। यह अधिकतर मनुष्य की थकान दूर करने की शारीरिक और मानसिक योग्यता पर निर्भर करती है। नींद व्यक्ति की प्रकृति, किये गये कार्य की मात्रा तथा उसके प्रकार पर निर्भर करती है। जो पूर्ण वयस्क हैं, उन्हें स्वयं ही अपने लिए आवश्यक नींद का निर्णय लेना चाहिए। "शीघ्र सोना और शीघ्र जागना मनुष्य को स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान् बनाता है।" इस बुद्धिमत्तापूर्ण उक्ति से दृढ़तापूर्वक लगे रहिए।
सोते समय सिर पूर्व में रखें। उत्तर की ओर सिर करके कभी न सोयें। आप अपना सिर पश्चिम की ओर करके भी सो सकते हैं। सोते समय मुँह न ढाँकें ।
दिन के समय नहीं सोना चाहिए। विशेषकर भोजन के बाद सोने से अपच और यकृत रोग हो सकते हैं।
खुले स्थान में सोने की आदत बहुत ही लाभदायक है। यदि आप सारी मांसपेशियों, मस्तिष्क और नाड़ियों को शिथिल कर सकें, तो आपको बिस्तर में लेटते ही तत्क्षण नींद आ जायेगी।
आपको यदि इस क्रिया का भली-भाँति ज्ञान है, तो आप काम करते भी विश्राम ले सकते हैं। जब बहुत से लोग बातें कर रहे हों, हँस रहे हों, हुए बैण्ड बज रहे हों, तो आप आरामकुर्सी पर बैठे-बैठे ही झपकी ले सकते हैं। कुछ क्षणों के शिथिलीकरण से आपके भीतर बहुत-सी ऊर्जा संग्रहित हो जायेगी। जो मानसिक रूप से शान्त है, वह किसी समय भी विश्राम कर सकता है, नींद ले सकता है। जो अच्छी तरह विश्राम कर सकता है, वह बहुत-सा काम कर सकता है। कार्य और स्थिति का परिवर्तन भी शिथिलीकरण या विश्राम ही है। आलस्य शिथिलीकरण से एकदम भिन्न है। ध्यान से पूर्ण विश्राम प्राप्त होता है।
सोने जाने से पहले आमाशय और मूत्राशय को खाली कर लें। यदि आप गहरी नींद चाहते हैं, तो आपको दिन के अन्तिम भोजन का समय नियमित करना होगा। यदि आप रात १० बजे सोना चाहते हैं, तो अपना 1 भोजन शाम ७ बजे समाप्त कर दें। यदि आप अपना भोजन सोने के तीन घण्टे पहले ग्रहण कर लेंगे, तो सोने से पहले तक भोजन का आधा पाचन हो चुकेगा और आप शान्तिपूर्वक सो सकेंगे।
सोने से पहले अपने दिन में किये गये कार्यों को स्मरण करें। अपनी आध्यात्मिक दैनन्दिनी भरें। अगले दिन के लिए नये संकल्प — जैसे ' मैं क्रोध पर नियन्त्रण करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कठोर शब्द या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं वासनाओं पर नियन्त्रण रखूँगा' आदि लें। आधा घण्टे जप करें। थोड़ी देर गीता, रामायण, भागवत या अन्य धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय करें। ये श्रेष्ठ आध्यात्मिक विचार आपके भीतर गहरे उतर जायेंगे। आप गहरी निद्रा का आनन्द उठायेंगे और बुरे स्वप्नों से मुक्त रहेंगे।
आप सर्वव्यापक परब्रह्म या अनन्त के साक्षात्कार द्वारा तुरीयावस्था, या चतुर्थ अवस्था में विश्राम कर जाग्रत निद्रा या निर्विकल्प समाधि के आनन्द का उपभोग करें और इस प्रकार स्वयं को सामान्य निद्रा जो अविद्या या अज्ञानता से उत्पन्न जड़ अवस्था है, से मुक्त करें।
गहन निद्रा-प्राप्ति के उपाय
१. चिन्ता करने की आदत छोड़ें। यह जीवन-शक्ति का धीरे-धीरे हास करती है। जो चिन्ता करता है, सो
नहीं सकता। ईश्वर पर विश्वास रखें । ईश्वर तथा उनके नाम में, उनकी कृपा में शरण लें। अपनी प्रार्थना और ध्यान में नियमित रहें। आपकी चिन्ता करने की आदत दूर हो जायेगी। आपको अच्छी विश्रान्तिदायक नींद आयेगी।
२. प्रसन्न रहें। सदा मुस्करायें। कीर्तन करें। ईश्वर की प्रार्थना करें। सारी चिन्ताएँ नौ दो ग्यारह हो
जायेंगी। आप अच्छी नींद सोयेंगे।
३. हलकी चादर का प्रयोग करें। बहुत से कम्बल ओढ़ कर न सोयें। भारी कम्बल आपकी नींद में बाधा
डालेंगे।
४. नींद लाने से लिए किसी औषधि का प्रयोग न करें, क्योंकि उनकी आदत बन जाती है। अफीम की ३०
बूँदें आपको पहले दिन थोड़ी नींद देंगी, किन्तु थोड़े दिन बाद आपको आधी बोतल से रंव मात्र भी निद्रा नहीं आयेगी। औषधियों से निराशा की भावना जन्मती है। प्राकृतिक विधियों से नींद लाने का प्रयास कीजिए।
५. पेट को अधिक न भरें। अपना भोजन हलका और शीघ्र पचने योग्य रखें। अपच अनिद्रा का एक कारण
है। अपना सायंकालीन भोजन ५ बजे समाप्त कर दें। इसमें कुछ फल और दूध ही लें। रात में कुछ न लें। आपको गहरी नींद आयेगी।
६. अपने मन और शरीर को पूर्ण शिथिल करें। निद्रा आपके पास आने हेतु बाध्य होगी।
७. आवेगपूर्ण विवादों, अनावश्यक तर्कों और विवेचनों को त्याग दें। अपने स्वभाव को नियन्त्रित रखें।
८. चाय-काफी को पूर्णरूपेण त्याग दें। वे मस्तिष्क और नाड़ियों की कोशिकाओं को अनावश्यक रूप से
उत्तेजित करती हैं।
९. उपन्यास, भूत की कहानियाँ, उत्तेजक, हत्या की कहानियाँ और उत्तेजक साहित्य न पढ़ें।
१०. किसी प्रकार के उत्तेजक पदार्थ न लें। मद्य, गांजा, अफीम आदि त्याग दें।
११. सोने से पहले कोई भी गम्भीर बुद्धि से सम्बन्धित काम न करे।
१२. मानसिक चंचलता या वाद-विवाद से बचें। सदा शान्त रहने का प्रयास करें। आवेगों पर नियन्त्रण रखें।
क्रोध पर नियन्त्रण रखें।
१३. उत्तेजना लाने वाले पदार्थ-गरम कढ़ी, चटनी, अत्यधिक मिर्च, इमली आदि न ग्रहण करें। अपना
भोजन रेशेदार और सादा रखें। फल और दूध का प्रयोग अधिक करें।
१४. सोने के ठीक पहले तेल-स्नान या सरसों का गरम पाद स्नान लें।
१५. सो कर उठते ही यह जानने का प्रयास न करें कि समय क्या हुआ है। इससे आप चिन्तित हो उठेंगे।
१६. सोने के कमरे में कोई प्रकाश न रखें। यदि आप प्रकाश के बिना सो नहीं सकते, तो कमरे में हरा प्रकाश
रखें।
१७. सोने के पूर्व सिर ब्राह्मी आँवला केश तेल लगायें।
१८. सोने के ठीक पहले १ कप गरम दूध में हार्लिक्स डाल कर पियें।
१९. सोने से पूर्व थोड़ा जप, प्रार्थना और ध्यान करें। कुछ शिक्षाप्रद पवित्र ग्रन्थों— जैसे गीता, योगवासिष्ठ,
उपनिषद्, भागवत, कुरान, बाइबिल आदि पढ़िए।
२०. मन को सुझाव दीजिए— “हे मन ! तुमने हर काम किया, तुमने सब-कुछ प्राप्त किया। किसी भी बात
की चिन्ता मत करो। अब तुम्हें कुछ करने और पाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण आराम से रहो। ध्यान करो। यह सम्पूर्ण जगत् मिथ्या है।” यह सुझाव आपको पूर्ण विश्रान्तिदायक निद्रा प्रदान करेगा और आपके मन को सभी चिन्ताओं से मुक्त करेगा।
२१. अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए। सभी कामनाओं और अभिलाषाओं को पूर्णरूपेण नष्ट करें।
कम बोलें। अधिक लोगों से मिलें-जुलें नहीं। अत्यधिक श्रम द्वारा स्वयं को न थकायें। अकेले सोयें। शाम को लम्बी सैर पर जायें।
२२. अपनी संकल्प-शक्ति का विकास करें। आत्म-संयम का अभ्यास करें। आप नेपोलियन और गान्धी जी
की भाँति अपने इच्छानुसार किसी भी स्थान पर, किसी भी समय सो सकते हैं और जिस समय चाहे जग सकते हैं।
२३. यदि आपकी नाड़ियाँ और मस्तिष्क कमजोर हैं, तो हलके प्राणायाम (ॐ के जप के साथ) के अभ्यास
द्वारा उन्हें शक्तिशाली और ऊर्जावान् बनायें। बादाम, ब्राह्मी की पत्तियाँ, मिश्री और काली मिर्च से बना पेय प्रात:काल पियें। ब्राह्मी घृत या हक्स्ले का नर्विगर सीरप लें।
२४. सोने के ठीक पूर्व सेन्टोजेन की एक खुराक लें, आपको अच्छी नींद आयेगी। आप प्रातःकाल दूसरी
खुराक ले सकते हैं। इसे दूध के साथ लें।
२५. शान्तिपूर्वक लेटें । मन और शरीर को शिथिल रखें। इससे आपको निद्रा की भाँति आरोग्यता प्राप्त
होगी। शान्तिपूर्वक ध्यान करने से आपको पूर्ण विश्राम प्राप्त होगा।
२६. सोने के ठीक पहले निम्न मन्त्र बोलें :
ॐ आस्तिकाय नमः, ॐ अगस्त्याय नमः, ॐ कपिलाय नमः,
ॐ मुचुकुन्दाय नमः, ॐ माधवाय नमः ।
ये पाँचों पुरुष अच्छी नींद सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका स्मरण करने से आपको बहुत अच्छी नींद आयेगी। इनमें से प्रथम तीन तो ऋषि हैं, अन्तिम भगवान् विष्णु हैं जो क्षीर सागर में योगनिद्रा में लीन रहते हैं और मुचुकुन्द भागवत में आते हैं।
सरसों का पाद-स्नान
गरम पानी एक टब में ले कर उसमें दो चम्मच सरसों का पिसा चूर्ण डाल लें। कुरसी या मोढ़े पर बैठ कर इसमें पैर डाल कर १५-२० मिनट बैठें। फिर पैरों को पानी में से निकाल कर सूखे तौलिये से पोंछ लें और मोजे पहन लें। अब सोने चले जायें। इससे आपको गहरी नींद आयेगी। यह सिरदर्द, चक्कर, गठिया, ज्वर आदि में भी बहुत उपयोगी है। यह पैरों को ठण्ढे होने से बचाता है।
शिथिलीकरण की क्रियाविधि
वर्तमान काल में जीवन अत्यन्त जटिल हो गया है, अस्तित्व के लिए संघर्ष बहुत अधिक बढ़ गया है। जीवन के प्रत्येक चरण में बहुत अस्वस्थ प्रतियोगिताओं का दौर है। रोटी की समस्या बहुत बढ़ गयी है। सभी जगह बेरोजगारी है। बुद्धिमान् नवयुवक जिनके पास विशिष्ट योग्यता और सिफारिश होती है, मात्र उन्हें ही आजकल रोजगार मिलता है। इस कारण आधुनिक मानव के ऊपर न समाप्त होने वाले दैनिक कामों तथा अस्वास्थ्यकर जीवन पद्धति के कारण निरन्तर शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता रहता है।
कार्य से गति उत्पन्न होती है, गति से आदत बनती है। मानव ने बहुत-सी कृत्रिम आदतें अपना ली हैं। उसने अपनी प्राकृतिक मूल आदतों को भुला दिया है। उसने गलत आदतों के द्वारा अपनी मांसपेशियों और नाड़ियों पर तनाव डाल दिया है। वह शिथिलीकरण के प्रथम सिद्धान्त को भूल गया है। उसे आज बिल्ली, कुत्ते और शिशु से शिथिलीकरण की क्रियाविधि सीखने की आवश्यकता है।
यदि आप शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे, तो आप अत्यन्त क्रियाशील तथा ऊर्जावान् होंगे । शिथिलीकरण में मांसपेशियाँ और नाड़ियाँ विश्राम की स्थिति में होती हैं। उनमें प्राण या ऊर्जा का संग्रहण और संरक्षण होता है। अधिकांश लोग जो शिथिलीकरण की इस सुन्दर क्रिया को नहीं जानते, वे मांसपेशियों और नाड़ियों पर अनावश्यक दबाव डाल कर, मांसपेशियों में अनावश्यक गति उत्पन्न करके अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते हैं।
कुछ लोग बैठे हुए अनावश्यक रूप से पैरों को हिलाते रहते हैं। कुछ लोग जब उनका मन बेकार या खाली होता है, अपनी उँगलियों से तबला बजाते रहते हैं। कुछ सीटी बजाते हैं। कुछ सिर हिलाते हैं। कुछ अपनी उँगलियों से छाती या पेट पर थाप देते हैं। शिथिलीकरण क्रिया के सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान न होने के कारण विभिन्न शारीरिक अंगों की अनावश्यक गतिविधियों द्वारा ऊर्जा का अपव्यय होता रहता है।
आलस्य को शिथिलीकरण समझने की भूल न करें। आलसी मनुष्य अकर्मण्य होता है। उसे काम करने में कोई रुचि नहीं होती। वह आलस्य और सुस्ती से पूर्ण रहता है। वह नीरस होता है। ऐसा मनुष्य जो शिथिलीकरण करता है तो वह मात्र विश्राम लेता है। उसमें शारीरिक बल, शक्ति, जीवनी शक्ति, सहन शक्ति होती है। वह थोड़ी मात्रा में भी ऊर्जा को व्यर्थ बहने नहीं देता । वह अद्भुत कार्य को सुन्दर ढंग से समय में सम्पन्न कर सकता है। बहुत ही कम
जब आप किसी काम को करने के लिए किसी मांसपेशी को सिकोड़ना चाहते हैं, तो मस्तिष्क से नाड़ी द्वारा उस मांसपेशी को तरंग भेजी जाती है। ऊर्जा या प्राण मुख्य प्रेरक नाड़ी द्वारा भेजा जाता है। फिर यह मांसपेशी तक पहुँचती हैं, और उसके अन्तिम छोर को खींचती है। जब मांसपेशी सिकुड़ती है, तो आप जिस पैर को चलाना चाहते हैं, उसे ऊपर खींचती है और आप इस क्रिया को सरलता से कर सकते हैं। पहले विचार आता है। यह विचार मांसपेशियों के संकुचन द्वारा क्रिया का रूप ले लेता है।
कल्पना कीजिए, आप एक कुरसी को उठाना चाहते हैं। यह इच्छा मन में एक तरंग उत्पन्न करती है। यह तरंग मस्तिष्क से प्रेरक नाड़ियों द्वारा हाथों की कोशिकाओं को भेजी जाती है। मस्तिष्क से नाड़ियों के साथ प्राण ऊर्जा भेजी जाती है, मांसपेशी सिकुड़ती है और आप कुरसी उठाने का कार्य कर पाते हैं। इसी प्रकार सभी कार्य आपके द्वारा चेतनावस्था या अचेतनावस्था में सम्पादित होते हैं। यदि मांसपेशियाँ बहुत श्रम कर लेती हैं. तो अधिक ऊर्जा व्यय होती है और आपको थकान का अनुभव होता है। अधिक श्रम, तनाव या खिंचाव के कारण प्राण या ऊर्जा का अधिक व्यय होता है जिससे मांसपेशियों को अधिक क्षति होती है।
जब आप किसी काम को चेतनावस्था में करते हैं, तो मन को एक सन्देश भेजा जाता है और मस्तिष्क आवश्यक अंग को प्राण ऊर्जा भेज कर तत्काल इस आदेश का पालन करता है। अचेतन अवस्था में काम सहज प्रेरणा से या यान्त्रिक रूप से होता है। मन तब आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता। जब एक बिच्छू आपकी उँगली पर दंश लगाता है, उंगली तुरन्त खींच ली जाती है। यह विवाद का विषय नहीं, यह सहज या यान्त्रिक प्रक्रिया है।
शीघ्र उत्तेजित होने वाला मनुष्य मन की शान्ति का उपभोग नहीं कर सकता। उसका मस्तिष्क, नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ सदा भारी तनाव में रहती हैं। वह अत्यधिक पेशी और नाड़ी-ऊर्जा तथा मानसिक शक्ति का अपव्यय करता है। ऐसा मनुष्य यदि शक्ति-सम्पन्न हो, तब भी वह अत्यन्त कमजोर मनुष्य है; क्योंकि वह अत्यन्त सरलता से अपना सन्तुलन खो देता है। यदि आप वास्तव में विघ्न रहित शान्ति और स्थाई सुख का आनन्द उठाना चाहते हैं, तो आपको चिन्ता, आकुलता, भय, क्रोध के आवेगों तथा दूसरे लोगों को दबाने वाली प्रवृत्ति को दूर कर अपने मन को शान्त, नियन्त्रित और सन्तुलित रखना होगा।
आप अनावश्यक रूप से चिन्ता करके, अकारण क्रोध करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्रोध पाशविक वृत्ति से जुड़ा हुआ है। क्रोध मस्तिष्क, रक्त और नाड़ियों को प्रत्यक्ष हानि पहुँचाता है। आपको क्रोध के प्रदर्शन से जरा भी लाभ नहीं होगा। किसी क्रिया को बार-बार करने से मन में एक आदत बन जाती है। यदि आप बार-बार चिन्ता करेंगे, चिन्ता करने की आदत बन जायेगी। चिन्ता, क्रोध तथा भय के द्वारा आपकी जीवन-शक्ति और ऊर्जा सरलता से बह जाती है। आप किसी भी बात से भयभीत क्यों होते हैं? जब कि सभी आपकी अपनी आत्मा हैं। भय, क्रोध और चिन्ता अज्ञानता की उपज हैं। क्रोध और चिन्ता के शिकार व्यक्ति की मांसपेशियाँ और नाड़ियाँ सदा संकुचित और तनाव में रहती हैं।
एक समूह की मांसपेशियों की क्रिया दूसरे समूह की मांसपेशियों द्वारा रोकी जा सकती हैं। एक तरंग एक समूह की मांसपेशियों को तुरन्त गति में लाने का प्रयास करती है। आप अन्य समूह की मांसपेशियों द्वारा प्रतिरोधक आवेग को भेज कर प्रथम समूह की मांसपेशियों की क्रियाविधि को रोक सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है, तो आप तत्क्षण ही कूद कर उसे मारने दौड़ पड़ते हैं। एक समूह की मांसपेशियों को बिना विचारे ही एकदम से काम करने का आदेश मिल जाता है; किन्तु आप उस आवेग को विवेक और परिवर्तन द्वारा कि 'मैं उसे मार कर कुछ प्राप्त नहीं करूँगा । वह एक अज्ञानी मनुष्य है। व्यवहार कैसे करना चाहिए, वह यह नहीं जानता। मुझे उसे क्षमा कर देना चाहिए।' उस आवेग को रोक सकते हैं। प्रतिरोधक आवेग तत्काल ही द्वितीय समूह की मांसपेशियों द्वारा प्रथम समूह की मांसपेशियों को काम करने से रोक देगा।
आवेगों और साथी आवेगों तथा प्रतिरोधी आवेगों में वृद्धि से नाड़ियों, मांसपेशियों और मस्तिष्क में भारी तनाव होता है। बहुत से लोग आवेगों के दास होते हैं, इसलिए वे मन की शान्ति का उपभोग नहीं करते।। वे इधर-उधर भटकते रहते हैं।
शिथिलीकरण की क्रिया एक सटीक विज्ञान है। यह अत्यन्त सरलतापूर्वक सीखा जा सकता है। मांसपेशियों के संकुचन की ही तरह मांसपेशियों का शिथिलीकरण भी महत्त्वपूर्ण है। मैं मन और नाड़ियों के शिथिलीकरण तथा मांसपेशियों के शिथिलीकरण पर बहुत अधिक बल देता हूँ। शिथिलीकरण के दो प्रकार हैं—शारीरिक और मानसिक । एक अन्य भी वर्गीकरण है आंशिक शिथिलीकरण— जब आप किसी भाग की कुछ मांसपेशियों को शिथिल करते हैं तथा पूर्ण शिथिलीकरण- जब आप सम्पूर्ण शरीर और मन की मांसपेशियों को शिथिल करते हैं।
शारीरिक शिथिलीकरण
दिन के समस्त कार्यों को समाप्त करने के बाद अपने शरीर की मांसपेशियों को किस प्रकार शिथिल किया जाये, इसका आपको अवश्य ज्ञान होना चाहिए। शरीर की मांसपेशियों को शिथिल करने से शरीर और मन को विश्राम प्राप्त होता है। शरीर का तनाव दूर हो जाता है। वे लोग जो शिथिलीकरण क्रिया का ज्ञान रखते हैं, वे ऊर्जा का अपव्यय नहीं करते। वे अच्छी तरह ध्यान कर सकते हैं।
आसनों और व्यायामों को पूर्ण करने के बाद नीचे चित लेट जायें। अपने हाथों को शरीर के बगल में पूरी तरह ढीले और शिथिल रखें। यह शवासन है। सिर से पैर तक समस्त मांसपेशियों को शिथिल कर दें। अपने मन को शीर्ष से पंजों तक घुमायें। आप पायेंगे कि कुछ मांसपेशियाँ अभी भी शिथिल नहीं हुई हैं, उन्हें भी शिथिल करें। शरीर को एक ओर दुलकायें और शीघ्र ही शिथिल हो जायें। किसी भी मांसपेशी को खींचें नहीं, पूर्ण शिथिल करें। अब इसी तरह दूसरी ओर शरीर को ढुलका दें और पुनः शिथिल करें। जब हम सोते हैं, तो ऐसा स्वयं ही होता है। शरीर की मांसपेशियों और विभिन्न अंगों के शिथिलीकरण हेतु बहुत से व्यायाम हैं। आप सिर, कन्धे, भुजाएँ, हथेली, कलाई, उँगलियों, पैरों, टखनों, एड़ियों, घुटनों, कोहनियों, कमर आदि को शिथिल कर सकते हैं। योगियों तथा मुक्केबाजों को शिथिलीकरण क्रिया का पूर्ण ज्ञान होता है। जब आप शिथिलीकरण के विभिन्न व्यायामों का अभ्यास करते हैं, तो मन में शान्त स्थिति और दृढ़ता का चित्र रखना चाहिए।
यदि आप चाहें, तो आसनों और व्यायामों के पश्चात् आरामकुरसी पर लेट कर भी शिथिलीकरण कर सकते हैं। जो शिथिलीकरण जानते हैं, वे जब चाहे थोड़ी देर १० मिनट की झपकी ले सकते हैं। व्यस्त लोगों, चिकित्सकों और वकीलों को शिथिलीकरण क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। वे रेलवे प्रतीक्षालयों, अदालत के कमरे में भी मन को शिथिल कर विश्राम कर सकते हैं। इस प्रकार वे अपने अगले काम के लिए तैयार हो सकते हैं। शिथिलीकरण मनुष्य को पूर्ण विश्रान्त कर देता है।
विद्यार्थी, पत्रकार, व्यस्त वकीलों, चिकित्सकों और व्यवसायी जनों को मानसिक शिथिलीकरण का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। जो इस आन्तरिक और बाह्य शिथिलीकरण की क्रियाविधि का ज्ञान नहीं रखते, वे अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का बहुत अधिक हास करते हैं। जो इस क्रिया का अभ्यास करते हैं, वे अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करके इसका प्रयोग अपने अधिकतम लाभ हेतु कर सकते हैं। योगियों को इस क्रिया का भलीभाँति ज्ञान होता है। वे इस विज्ञान के पूर्ण स्वामी होते हैं। जो इस क्रियाविधिक अभ्यास करते हैं, उन्हें कभी थकान का अनुभव नहीं होता। वे खड़े-खड़ ही कुछ क्षणों के लिए आँखें बन्द करके स्वयं को आगामी कार्य हेतु तैयार कर लेते हैं। जिस प्रकार नल खोलने से पानी प्रवाहित होता है, उसी प्रकार शिथिलीकरण करने से ऊर्जा नाड़ियों में प्रवाहित होती है।
वे स्त्रियाँ जो कभी शिथिलीकरण नहीं करतीं, कभी भी सही ढंग से विश्राम नहीं कर पातीं और उनका सौन्दर्य बना नहीं रह सकता। उनके मुख पर उनका शरीर जिस थकावट का अनुभव कर रहा है, उसके स्पष्ट चित्र दिखायी देते हैं। उनका शरीर भारहीन हो जाता है। निरन्तर नाड़ी-तनाव की स्थिति में रहने के कारण (जैसा कि सामान्यतया स्त्रियाँ रहती हैं) वे समय में पूर्व ही बूढ़ी हो जाती हैं, अपना सौन्दर्य खो देती हैं और बाद में वे पाती है। कि तनाव ने उनकी सारी शक्ति को क्षीण कर दिया है।
चाहे काम कितना ही आवश्यक क्यों न हो, प्रातःकाल और मध्याह में कम-से-कम १० मिनट के लिए पूर्ण शिथिलीकरण करें। इस नियम में सदा दृढ़ रहें। किसी भी बहुत आरामदेह कुरसी पर बैठ जायें या गद्दे पर चित लेट जायें, अपने पैरों में घुटनों के नीचे कुशन रख कर पैरों को भूमि से १८ इंच उठा दें, प्रत्येक मांसपेशी को ढीला छोड़ दें।
यदि आप गद्दे पर लेटे हैं, तो सिर के नीचे एक तकिया रख लें। इससे गले की मांसपेशियों को शिथिल करने में सहायता होगी। आँखें बन्द कर लें और मन को रिक्त करें।
पैरों को ऊपर उठा देने से रीढ़ सीधी रहती है और पैरों से रक्त नीचे की ओर चला जाता है जिससे वे ठण्ढे रहते हैं। जब आप कुरसी पर विश्राम करें, पैरों को सहारा दे दें और प्रत्येक मांसपेशी को शिथिल करें। यह पहले तो करने में कठिन प्रतीत होता है; पर बाद में इसकी आदत बन जायेगी।
बहुत से ऐसे काम हैं जो बैठे-बैठे किये जा सकते हैं—जैसे कपड़ों पर रफू करना, मरम्मत करना और सिलाई मशीन का काम आदि। बैठते समय सावधानी रखें, ताकि थकावट न हो। मात्र कुछ स्त्रियों को इस तथ्य की जानकारी है कि बैठने की सही स्थिति न होने से कूल्हे मोटे हो जाते हैं। कुरसी के किनारे पर न बैठें, शरीर को अच्छी प्रकार से पीछे टिका कर बैठें और शरीर के निम्न भाग को सहारा देने के लिए एक स्थिर कुशन का प्रयोग करें। दूसरी बात याद रखने की यह है कि कुरसी सही ऊँचाई की होनी चाहिए। घुटने पर घुटना चढ़ा कर नहीं बैठना चाहिए, न ही पैरों को चौड़ा करके बैठना चाहिए। घुटनों और पैरों को पास-पास रखें तथा उन्हें भूमि या मेज पर स्थिर जमा कर रखें।
खड़े होने की सही स्थिति से भी थकान से बचा जा सकता है। यदि आपका काम ऐसा है कि आपको अधिक देर खड़ा रहना पड़ता है, तो आप अपने घुटनों और एड़ियों को परस्पर जोड़ कर खड़े हों। इससे एक खम्भा-जैसा बन जाता है, जिस पर शरीर विश्राम कर सकता है। शरीर के भार को एक पैर से दूसरे पर नहीं डालते रहना चाहिए; बल्कि इसे दोनों पर समान रूप से वितरित करना चाहिए ।
मानसिक शिथिलीकरण
जिस प्रकार आप आसनों और शारीरिक व्यायामों के बाद अपनी मांसपेशियों को शिथिल करते हैं, आपको उसी प्रकार एकाग्रता, ध्यान, स्मृति के अभ्यास, संकल्प-शक्ति के विकास के अभ्यास के बाद मन को ल करके विश्राम करना चाहिए। मन के शिथिलीकरण से शरीर को भी विश्राम मिलता है। शरीर और मन का अन्तरंग सम्बन्ध है। शरीर मन के द्वारा उसके आनन्द के लिए बनाया हुआ ढाँचा है।
मन शरीर द्वारा अनुभव करता है और प्राण इन्द्रियों और शरीर के संयोग से काम करता है। मन शरीर पर प्रभाव डालता है। यदि आप प्रसन्न रहेंगे, शरीर भी शक्तिशाली होगा। जब आप हताश रहते हैं, शरीर काम नहीं कर सकता। इसके विपरीत शरीर भी मन पर कुछ प्रभाव डालता है। यदि शरीर शक्तिशाली है, स्वस्थ है, तो मन भी प्रसन्न और बलवान् होगा — जैसे यदि पेट में दर्द होता है, तो मन भी काम नहीं कर सकता। विचार कार्य रूप में परिणित होते हैं और मन पर प्रतिक्रिया करते हैं, मन शरीर पर कार्य करता है और शरीर मन पर प्रतिक्रिया करता है। मांसपेशियों का तनाव दूर करने से मन पूर्वावस्था को प्राप्त हो कर शान्त हो जाता है।
शिथिलीकरण द्वारा आप मन को, थकी हुई नाड़ियों और अत्यधिक श्रम के द्वारा थकी हुई मांसपेशियों को विश्राम प्रदान करते हैं। आपको मन की आन्तरिक शान्ति, शक्ति, ओज, शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त होता है। मन का शिथिलीकरण करते समय मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के बाहरी विचार नहीं होने चाहिए। क्रोध, निराशा, असफलता, अनिच्छा, कष्ट, दुःख, विवाद - ये सभी आन्तरिक और मानसिक तनाव के कारण हैं। मन का शिथिलीकरण करने से मानसिक तनाव दूर हो जाता है और मन नयी मानसिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है और इससे आपको प्रसन्नता और सुख प्राप्त होता है। चिन्ता और क्रोध अगर दूर कर दिये जायें, तो मन का सन्तुलन और शान्ति प्राप्त की जा सकती है।
चिन्ता और क्रोध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इनके भीतर ही भय भी छुपा हुआ है। इनसे हमारी बहुत-सी ऊर्जा व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। सदा सावधान और विचारवान् बनें। सभी प्रकार की अनावश्यक चिन्ताएँ दूर कर दें। समस्त भय, चिन्ता, क्रोध को बाहर निकाल दें। साहस, प्रसन्नता, आनन्द, शान्ति तथा सन्तुष्टि के बारे में विचार करें। १५ मिनट तक आरामदायक स्थिति और सहज स्थिति में बैठें। आँखें बन्द कर लें। अपने मन को बाहरी वस्तुओं से वापस खींच लें। अपने मन में उबलते विचारों को शान्त करें।
आँखें बन्द करें। किसी सुखकर वस्तु के बारे में सोचें। यह मन को आश्चर्यजनक ढंग से शिथिल करेगा। विशाल हिमालय, पवित्र गंगा या कश्मीर के किसी आकर्षक दृश्य के बारे में, ताजमहल, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल, सुन्दर सूर्यास्त, बड़ा विस्तृत समुद्र या अनन्त नीले आकाश के बारे में सोचें। आप सोचें कि इस ब्रह्माण्ड महासागर में सारा जगत् और आपका शरीर तिनके की भाँति तैर रहा है। अनुभव करें कि आप परमात्मा के सम्पर्क में हैं। अनुभव करें कि इस सम्पूर्ण जगत् का जीवन स्फुरित, कम्पित और स्पन्दित हो रहा है। अनुभव करें कि भगवान् हिरण्यगर्भ, जीवन धन, आपको अपने बृहत् वक्षस्थल में धीरे-धीरे झूला झुला रहे हैं। अब अपनी आँखें खोलें। आपको बहुत अधिक मानसिक शान्ति, मानसिक बल और मानसिक शक्ति का अनुभव होगा। इसका अभ्यास करें और अनुभव करें।
उत्तर दिशा की ओर सिर करके न सोयें
उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना लगभग सभी भारतीयों में निषिद्ध है। हिन्दुओं में यह प्राचीन परम्परा है। विश्वव्यापी रूप से प्रत्येक विचारवान् हिन्दू जो अपने रीति-रिवाजों का थोड़ा भी सम्मान करता है, ऐसा करने से बचता है। किन्तु इसके लिए कोई बुद्धिमत्तापूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी न होने के कारण विश्व में लोग इसे अनावश्यक मानते हैं। किन्तु एक विवेकी और स्पष्ट बुद्धि वाले हिन्दू का सामान्य ज्ञान कहता है कि प्रकट में तुच्छ दिखायी पड़ने वाली इन रीतियों के पीछे कोई-न-कोई ठोस कारण अवश्य होगा; क्योंकि इन्हें हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने बताया है, जिन्होंने अपनी विचार-शक्ति द्वारा आत्मिक दृष्टि का विकास किया और ऐसे सूक्ष्म बलों (जो हमें भौतिक नेत्रों से नहीं दिखायी देते) के कार्यों को अनुभूत किया।
अब यह सिद्धान्त या नियम जन-समूह के द्वारा स्पष्ट अनुभूत किया जा चुका है। यदि किसी को कहा जाये कि कोई विशेष काम नहीं करना चाहिए, तो उस बात का उस व्यक्ति पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि वह बात सुनते ही भुला दी जाती है। किन्तु यही तथ्य कुछ प्रबुद्ध लोगों द्वारा उठाये जायें और उन्हें जन-सामान्य को बताया जाये, तो फिर वही व्यक्ति उसे स्वीकार लेता है। यह मानव की कमजोरी है और हमारे प्राचीन ऋषि मानव की इस निर्बलता से अच्छी तरह परिचित थे । वे बहुत चतुर मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अपना सारा ज्ञान तथा अपने समस्त अन्वेषणों की शिक्षा भय उत्पन्न करने वाली असामान्य घटनाओं तथा कुछ मनोवैज्ञानिक कहानियों और दृष्टान्तों के रूप में दी है ।
जैसे भगवान् श्री गणेश जी की कहानी में बताया है कि एक हाथी उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोया था जो कि एक भयंकर भूल है। इसीलिए उसका सिर काट कर गणेश जी के गले पर लगा दिया गया। यह घटना यह दर्शाती है कि उत्तर दिशा हेतु निषेध आर्यों के समय भी प्रचलित था। यह तथ्य कि यह रीति सदियों से चली आ रही है और आज भी दृढ़ है। हमें यह विश्वास करने को बाध्य करती है कि यह कल्पना या अज्ञानता पर आधारित नहीं है। हिन्दू सभ्यता सदा आवश्यक रूप से प्रगतिशील रही है और उसके ऐसे मौलिक सुधारक तथा निर्दय आलोचक भी बहुत हैं जो किसी बात की छानबीन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते, बहुत कम लोग ही उनकी पैनी सूक्ष्म दृष्टि से बच पाते हैं और ऐसे रीति-रिवाज उनके दृष्टिकोण में पूर्ण निरर्थक हैं और इसलिए बहुत पहले ही विस्मृत कर दिये गये हैं।
जो लोग इस नियम को नहीं जानते और उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं और उन्हें इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती, यदि वे अपनी आदत बदल लें, तो वे दिशा बदलने के लाभ को जान सकेंगे। जब तक मनुष्य किसी गलत आदत को त्याग कर उसकी विपरीत सही आदत को अपना न ले, वह गलत आदत से होने वाली हानि के प्रति जाग्रत नहीं होता। आदत बदलने पर ही वह उसके लाभ को जान सकता है, अनुभव कर सकता है।
उपनिषदों के ऋषियों ने जो सिद्धान्त बताये प्राचीन काल से ही उनका प्रभाव अविवादित रहा है। कुछ नियम जैसे 'सन्ध्या के समय सोना नहीं चाहिए, गणेश चतुर्थी पर चन्द्रमा नहीं देखना चाहिए, ग्रहण के समय कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए' आदि ये सभी ऋषियों ने अन्तरिक्ष और अन्य लोकों में कार्यरत सूक्ष्म बलों के अध्ययन द्वारा बनाये हैं। मनुष्य दैहिक रूप से ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट ब्राह्मिक सूक्ष्म शरीर रखने के कारण एक जटिल प्राणी है और सूक्ष्म बलों के कार्य के प्रति अति संवेदनशील है। इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने उसके कल्याणमय जीवन हेतु ये व्यवस्थाएँ दी हैं।
पश्चिमी वैज्ञानिक बाह्य प्रकृति के कार्यों का अत्यन्त सूक्ष्म परीक्षण करते हैं और चौंकाने वाले अन्वेषण करते हैं; किन्तु आज भी वे प्राचीनकालीन पूरब के लोग जिन सटीक सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते थे, उनका परीक्षण करने के पूर्णरूपेण योग्य नहीं हुए हैं। आधुनिक विज्ञान कारण और अवलोकन पर आधारित है; किन्तु इस उद्देश्य हेतु यह मानव-मन नामक यन्त्र जिसमें स्वयं ही समस्त विशिष्ट दोष हैं, अत्यन्त सीमित है। वास्तव में प्राचीन काल ऋषि आधुनिक विज्ञान से अति-आधुनिक और आधुनिक वैज्ञानिकों से महान् वैज्ञानिक थे। ये ऋषि ऐसे शोध करने वाले विद्यार्थी थे जो प्रयोगशालाओं के बिना शोध करते थे। वे मनुष्य द्वारा सजाये गये उपकरणों से नहीं, वरन् ईश्वर द्वारा दी गयी सुविधा — अन्तर्ज्ञानात्मक बुद्धि, संयम द्वारा शुद्ध दुर्बोध बुद्धि, अनुशासन, नियमितता के अभ्यास के द्वारा शोध करते थे। वे सूक्ष्म ग्रहों की गहराई में जा कर उन आन्तरिक सिद्धान्तों पर विचार करते थे जो गुप्त रूप 'कार्य करते हैं और इस भौतिक दृश्यमान् जगत् पर शासन करते हैं। मात्र अन्तर्ज्ञान ही मन से परे सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक ग्रहण करता है। अवलोकनों और प्रयोगों से परे जो सिद्धान्त होता है, वह सत्य तक आंशिक रूप से पहुँचने हेतु श्रेष्ठ है। इसमें कोई भूल नहीं होती। यह वह एकमात्र बोधज्ञान और अनुभव है, जो किसी भी निश्चित घोषणा हेतु अन्तिम स्रोत है।
अधिकांश नयी विचारधारा के प्रवर्तक चीख-चीख कर कह रहे हैं— “उपनिषदों की ओर वापस जाओ।" इस साहसिक पुकार से निस्सन्देह यह सिद्ध होता है कि उपनिषदों के ऋषि मात्र स्वप्नद्रष्टा नहीं थे। यह दुन्दुभि किसी पुरातन संन्यासी ने नहीं बजायी है; बल्कि यह उन ज्ञानी, स्वच्छ मति वाले ऋषियों द्वारा बजायी गयी है, जो पश्चिमी जीवन और सभ्यता के शिखर पर थे और प्रत्येक बात को अत्याधुनिक निर्माताओं के निष्पक्ष और न क्षमा करने योग्य दृष्टिकोण से परखते थे।
इसीलिए यह देखा गया है कि प्रचलित परम्पराओं में विश्वास करना और उनका विश्वास सहित अवलोकन करना आवश्यक और लाभदायक भी है। वे अन्धविश्वास नहीं, वरन् मानव के कल्याण हेतु, हमारी रक्षा के लिए ठोस व्यवस्थाएँ हैं। मानव के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह ज्ञान के प्रत्यक्ष अवग्रहण और अनुभव के साथ ऋषियों के द्वारा बनाये गये इन नियमों में दृढ़ रहे। हमारे लिए हर बात के लिए यह पता लगाना कि ऐसा क्यों? किसलिए? सदा लाभदायक नहीं होता। कुछ बातें बिना प्रश्न किये अनिवार्य रूप से सदा मानी जानी चाहिए।
यह सम्भव है कि उत्तर दिशा की ओर सिर न करके सोने का मुख्य आधार यह है कि प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह को वक्षस्थल और उदर के क्षेत्र में मुक्त बनाना; क्योंकि यह इस क्षेत्र में रात के समय कोशिकाओं के पुनर्निर्माण और आरोग्य-प्राप्ति हेतु बहुत आवश्यक है। दिन में जब हम जागते रहते हैं, मन और मस्तिष्क पूर्ण और निरन्तर काम करते रहते हैं और वे सम्पूर्ण प्राणिक ऊर्जा का स्वतन्त्र रूप से उपयोग कर लेते हैं। किन्तु रात के समय मस्तिष्क विश्राम करता है तथा मन भी तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील रहता है तथा नेत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय काम नहीं करती; इसलिए प्राणिक ऊर्जा बचे हुए संस्थान की ओर प्रेरित होती है। (अर्थात् उदर-क्षेत्र की ओर) । साथ-ही-साथ यदि सिर उत्तर की ओर होगा, तो उत्तर दिशा से आ रही चुम्बकीय तरंगों के खिंचाव के कारण प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा पड़ेगी; क्योंकि यह सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से सदा चुम्बकीय तरंगें निकलती रहती हैं और इनके कारण प्राणिक ऊर्जा जिसे उदर क्षेत्र की ओर जाना है, उसे इस चुम्बकीय खिंचाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उसे दोहरा काम करना पड़ता है। इस दोहरे कार्य से बचाव हेतु, प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह को सरल, सुगम बनाने के लिए मनुष्य को उत्तर दिशा में सिर करके सोना निषिद्ध किया गया है। सबसे अच्छा तो यह है कि आप पूर्व दिशा में सिर करके सोयें।
निद्रा और सत्त्व
जब आप सोने जायें,
आपके भीतर सत्त्व होना चाहिए।
आपको तभी अच्छी नींद आयेगी।
यदि आपके भीतर रज होगा,
आपको निद्रा में बाधा पड़ेगी।
जब आप अगले दिन प्रातः उठेंगे,
आप विश्रान्त नहीं हो पायेंगे।
यदि आप तम से पूर्ण होंगे,
जब आप जागेंगे,
आपको भारीपन, सुस्ती और नीरसता का अनुभव होगा।
इसलिए सोने जाने के पहले ध्यान और जप करें।
नींद और समाधि
मोक्षप्रिय बोला-
हे पुरुषोत्तम, अब मैं समाधि के तत्त्व और प्रकृति को समझ गया हूँ। क्या अब मैं निद्रा और समाधि के मध्य अन्तर को जान सकता हूँ?
स्वामी शिवानन्द जी ने उत्तर दिया-
तुमने ठीक कहा, हे मोक्षप्रिय ! यह एक बहुत सुन्दर प्रश्न है। इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य ही दूँगा ।
निद्रा एक जड़ अवस्था है; लेकिन समाधि शुद्ध चेतना या शुद्ध जाग्रति की स्थिति है।
जब एक मनुष्य निद्रा से वापस आता है, तो उसे आत्मा के अनुभवातीत ज्ञान का कोई अनुभव नहीं होता। वह भारी और सुस्त अनुभव करता है । किन्तु जब एक योगी या साधक समाधि की अवस्था से वापस आता है, वह आत्मा के परम श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त रहता है। वह आपको प्रेरणा प्रदान करता है और ऊँचा उठा सकता है। वह स्वयं ही ब्रह्म है।
समाधि जाग्रत निद्रा है। साधक को बाह्य जगत् की कोई चेतना नहीं होती। वह ज्ञानानन्द के सागर में लीन रहता है।
हे मोक्षप्रिय, निद्रा में गहन तम होता है। जीवात्मा कारण शरीर में विश्राम करती है; किन्तु समाधि में वह ब्रह्म या सच्चिदानन्द स्वरूप में विश्राम करती है।
यदि आप जग जाते हैं, तो गहन निद्रा की अवस्था अदृश्य हो जाती है। इस कारण जो ऐसी परिवर्तनशील अवस्था है, वह माया या मिथ्या है। किन्तु समाधि या परम चेतनावस्था तीनों अवस्थाओं की साक्षी चेतनावस्था है। यह सदा स्थाई है और इसी कारण यह ही एकमात्र सत्य या यथार्थ अवस्था है।
निद्रा में वासनाएँ और संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहतें हैं; किन्तु समाधि में ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं।
हे मोक्षप्रिय ! अपने अहंकार, वासनाओं और पाँचों इन्द्रियों को भस्म कर दो और इस निद्रा समाधि का आनन्द उठाओ।
एक भिक्षुक और सम्राट् की निद्रा में कोई अन्तर नहीं होता।
नींद में प्राप्त होने वाला सुख दोनों के लिए एक सदृश है।
नींद में आप संसार का कष्ट, रोग का दर्द, दुःख आदि भूल जाते हैं।
निद्रा का सुख ऋणात्मक नहीं है।
यह वास्तव में धनात्मक है।
निद्रा का आनन्द उठाने के लिए लोग बहुत-सी तैयारियाँ करते हैं जैसे नर्म बिस्तर, तकिया, खटिया आदि।
निद्रा का सुख वास्तव में आत्मा का आनन्द है।
किन्तु निद्रा में आवरण होता है।
इसीलिए मनुष्य कहता है-"मैं नींद में कुछ नहीं जानता।"
निद्रा में सुख अज्ञानता से मिला हुआ होता है।
यदि वहाँ अज्ञान या आवरण न हो
तो आप समाधि के आनन्द का उपभोग करेंगे।
तपस्या और यन्त्रणा
आप बिना भोजन के थोड़े दिन रह सकते हैं। आप पानी के बिना थोड़े दिन रह सकते हैं; किन्तु आप नींद के बिना थोड़े दिन भी नहीं रह सकते। नींद या विश्राम प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है।
ईश्वर ने तो हमारे आन्तरिक अंगों जैसे हृदय तक के लिए भी विश्राम हेतु व्यवस्था दी है। दोनों धड़कनों के मध्य हृदय थोड़ा विश्राम लेता है। इसी कारण यह जन्म से मृत्यु तक बिना रुके काम करता है। ऐसा ही फेफड़ों के साथ भी है। जो योगी कुम्भक करते हैं, उनके जीवन काल में वृद्धि हो जाती है, उसका भी यही रहस्य है। समाधि में फेफड़ों को पूर्ण विश्राम मिलता है।
गहन निद्रा में मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान विश्राम लेते हैं। दिन में वे सतत क्रियाशील रहते हैं। रात में वे विश्राम ले कर अगले दिन के लिए ऊर्जा और शक्ति पुनः प्राप्त करते हैं। यदि वे इस विश्राम हेतु मना कर दें, तो वे काम करना बन्द कर देंगे। जिस प्रकार भूख और प्यास के कारण कष्ट होता है, उसी प्रकार निद्रा न मिलने से भी कष्ट होता है।
प्राचीनकाल में अपराधी को यन्त्रणा के रूप में उसे सोने नहीं दिया जाता था। जब उसे कई दिनों तक जगाये रखा जाता था, तो वह दु:खी हो कर अपना अपराध स्वीकार कर लेता था या रहस्य उगल देता था। नींद न होने से मन और इन्द्रियाँ अपनी शक्ति खो देती हैं और अत्यन्त दुर्बल हो जाती हैं।
पूर्वकाल के तपस्वी इस रहस्य को जानते थे; इसलिए वे मन और इन्द्रियों को वश में करने के लिए इस उपाय का प्रयोग करते थे और वे नींद को वश में करने के लिए अत्यन्त कठिन उपायों को अपनाते थे। क्योंकि उनके पास अत्यन्त प्रबल संकल्प शक्ति और महान् आध्यात्मिक शक्ति थी तथा उनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण और सूक्ष्म थी; इसलिए वे मन और इन्द्रियों के पूर्ण वशीकरण द्वारा आध्यात्मिक लाभ उठाते थे। जब इन्द्रियाँ मृत हो जाती हैं और मन क्षीण हो जाता है, तो योगी आत्मारूपी बहुमूल्य गहने को इन दोनों चोरों (मन और इन्द्रियों) से पुनः प्राप्त कर लेता है।
इस युग में मनुष्यों के पास ऐसी प्रबल संकल्प-शक्ति नहीं है; इसलिए ऐसी तपस्या उनके लिए अनुकूल नहीं होगी। इस कारण भगवान् श्री कृष्ण ने भगवद्गीता में ऐसे कठोर अभ्यास हेतु मना किया है। उन्होंने साधकों को आहार और सोने में संयम बरतने के लिए कहा है। उन्होंने अन्य प्रकार की तपश्चर्या बतायी है जैसे वाणी का तप, शारीरिक तप तथा मानसिक तप, ये सभी इस युग में भी सबके लिए अति अनुकूल हैं।
अपनी वाणी को संयमित कीजिए, अपने शरीर पर नियन्त्रण रखिए, मन का संयम कीजिए, विचारों, कार्यों और आवश्यकताओं को संयमित कीजिए और इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त कीजिए ।
लयबद्धता
वे परिस्थितियाँ जो ध्यान करने वाले साधक में मन की पूर्ण एकाग्रता लाती हैं, वे ही सामान्य मनुष्य में गहन निद्रा लाती हैं।
गहन निद्रा तथा मन की पूर्ण एकाग्रता — दोनों में मन केन्द्रित रहता है। गहन निद्रा में प्रज्ञा आत्म अवशोषित और एक सदृश तथा जाग्रत तथा स्वप्नावस्था में जिसके सात पैर और नौ मुख होते हैं, उस विश्व और तेजस से भिन्न होती है। गहन निद्रा में अज्ञानता का आवरण होता है। यदि यह आवरण हट जाये, तो आप गहन निद्रा के स्थान पर समाधि का आनन्द उठायेंगे।
समाधि और गहन निद्रा —दोनों ही अवस्थाओं में बाह्य वस्तुओं के साथ संयोजन नहीं रहता, उसमें राग-द्वेष की प्रवृत्तियाँ नहीं रहतीं और अनुभव लगभग एक समान रहते हैं। गहन निद्रा में किसी के प्रति जागरूकता नहीं होती; किन्तु समाधि में पूर्ण आत्म- जागृति रहती है।
सभी साधक जानते हैं कि मन की एकाग्रता हेतु लयबद्धता अत्यन्त सहायक होती है। घड़ी की लयबद्ध टिक-टिक की ध्वनि, स्टोव की लयबद्ध ध्वनि, बहती हुई नदी की लयबद्ध ध्वनि, संगीत के उपकरण के किसी एक स्वर की लयबद्ध ध्वनि, बिजली के पंखें की लयबद्ध ध्वनि-ये सभी यदि ध्यानपूर्वक सुनी जायें, तो मन की एकाग्रता या गहन निद्रा हेतु सहायक होती हैं।
ऐसी एक लय से आती ध्वनियों में अपनी रुचि बढ़ायें और उन्हें सम्पूर्ण हृदय और आत्मा से सुनें। धीरे-धीरे यह जगत् आपके भौतिक और मानसिक नेत्रों के सामने अदृश्य हो जायेगा और आप निद्रा देवी की गोद में चले जायेंगे। आप जितना अधिक ध्यान से उन ध्वनियों को सुनेंगे, आप उतनी ही गहरी नींद प्राप्त कर सकेंगे। धीरे-धीरे यह ध्वनि सम्पूर्ण जगत् लील जायेगी और आपके मन से सारे विचारों को बाहर निकाल देगी और आपको पूर्णरूपेण रिक्त कर देगी। तब आपको गहरी नींद आ जायेगी।
किसी विशेष मन्त्र का जप करने में भी यही सिद्धान्त काम करता है। एक बड़ी दर्शन की पुस्तक पढ़ने के स्थान पर मन्त्र-जप पर बहुत अधिक बल दिया जाता है और बड़े मन्त्रों के स्थान पर छोटे मन्त्र का चुनाव किया जाता है। मन्त्र जितना छोटा होगा, उसमें उतनी अधिक अखण्ड लयबद्धता उत्पन्न होगी और मन अत्यन्त शीघ्रता से एकाग्र हो सकेगा।
देखिए, जब आप घड़ी की टिक-टिक पर मन को एकाग्र करते हैं, तो क्या होता है—
कुछ समय तक तो आप टिक-टिक सुनते हैं, तो आपको यह चेतना रहती है कि यह ध्वनि आपके बिस्तर के पास रखी घड़ी से आ रही है। आप प्रसन्नतापूर्वक टिक-टिक की ध्वनि को सुनते जाइए। अचानक आपको लगेगा कि यह ध्वनि आपके भीतर से भी आ रही है। अब आपका ध्यान बाहर से हट जायेगा और आपके भीतर से आ रही टिक-टिक की ध्वनि पर केन्द्रित हो जायेगा और आपको अब मुश्किल से ही मालूम पड़ सकेगा कि घड़ी और उसकी टिक-टिक को क्या हुआ ? आप जब जागेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत गाढ़ी नींद आयी ।
इस विषय में घड़ी की टिक-टिक (उदाहरण के लिए इसका यहाँ प्रयोग हुआ है) चेतना की दो अवस्थाओं से जाती है (या आपको ले जाती है) प्रथम तो आप इसे बाहर से सुनते हैं—जाग्रत अवस्था, दूसरी जब आप इसे भीतर सुनते हैं, जब आपके भीतर आपके मन द्वारा निर्मित घड़ी टिक-टिक करती है—वह है स्वप्नावस्था । इस समय गहन निद्रा आती है।
एकाग्रता मन और इन्द्रियों की मृत्यु है। एकाग्रता का अभ्यास करें, आप गहन निद्रा का आनन्द उठा सकेंगे। आप अपना काम पूर्ण दक्षता से कर सकेंगे। आप अपनी साधना में शीघ्र प्रगति करेंगे। आप इस जीवन में नहीं, इसी क्षण भगवद्-साक्षात्कार करेंगे।
इच्छा-शक्ति निद्रा प्राप्त करना
अपनी इच्छा के अनुरूप सोना और जागना अर्थात् मन के ऊपर सजगतापूर्वक नियन्त्रण, जिसके द्वारा व्यक्ति इसे अपनी इच्छानुसार परिवर्तित कर सके।
व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं सो पाता? इसका उत्तर जब आप पूरी तरह यह जान लेंगे कि वास्तव में सोना क्यों पड़ता है? तभी दे पायेंगे।
दिन में दस इन्द्रियाँ काम करती हैं—पाँच कर्मेन्द्रियाँ जो शरीर को काम के समय क्रियाशील रखती हैं तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ जो ज्ञान और अनुभूतियाँ एकत्र करती हैं। ये सभी सूक्ष्म इन्द्रियाँ जिन भौतिक साधनों का प्रयोग करती हैं, वे नाशवान् पदार्थों से निर्मित हैं और ऐसी वस्तु जो समय पा कर नष्ट हो जाती है, वह स्वाभाविक रूप से क्षति और नाश की ओर ले जायी जाती है।
जीव तीन ग्रन्थियों— अविद्या, काम और कर्म से बँधा होने के कारण ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ग्रहण करता है और दिन के समय कार्य करता है। अविद्या प्रारम्भिक अज्ञान है, कामना इसका परिणाम है और कर्म इस कामना के परिणाम हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कामना पर सभी कर्मों का अत्यधिक भार है। अज्ञानी जीव कामना जो कि अविद्या का प्रतिफल है, उसकी पूर्ति के लिए इन्द्रियों द्वारा कर्म करता है।
दिन समाप्त होने पर जब नाशवान् इन्द्रियाँ क्षीण हो जाती हैं और काम नहीं कर सकतीं, तो जीव उन्हें त्याग देता है, तब मनुष्य स्वयं को संवेदनाशून्य स्थिति में बिस्तर पर डाल देता है। अभी भी मन में या अन्य सूक्ष्म इन्द्रियों में थोड़ी संचित ऊर्जा शेष रहती है। यह जीव जो कि इन अविजित इन्द्रियों के आगे विवश रहता है, इन सूक्ष्म इन्द्रियों और मन पर काम करते रहने के लिए दबाव डालता है। यह स्वप्नावस्था होती है। जब यह संचित ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, तब इन्द्रियाँ और मन जीव की गोद में वापस आ कर अधिक ऊर्जा के लिए पुकारते हैं। यह गहन निद्रा की अवस्था होती है। इसमें मन और इन्द्रियाँ अपने वास्तविक स्रोत आत्मा से ऊर्जा ग्रहण करती हैं जो कि आवरण से ढकी हुई हैं।
अब आप कामनाओं के प्रबल वेग, इन्द्रियों पर पड़ने वाले दबाव, नींद की महान् अनिवार्यता और अनिद्रा की सम्भाव्यता को समझ गये होंगे। कामना की प्रबलता मन और इन्द्रियों को प्रेरित करके जब तक उनकी ऊर्जा की अन्तिम बूँद बह नहीं जाती, तब तक उन्हें काम में लगाये रखती है। वह मनुष्य जो कामनाओं से भरा रहता है, वह सदा उत्तेजित रहता है और उसका मस्तिष्क सदा विचारों और आवेगों की तरंगों द्वारा आन्दोलित होता रहता है। वह विश्राम और शान्ति को नहीं जानता। कोई भी यह सोच सकता है कि ऐसे व्यक्ति को बड़ी गहरी नींद आनी चाहिए; किन्तु नहीं, एक फटेहाल व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से अधिक गहरी नींद सोता है और यह व्यक्ति इतनी गतिविधियों के बाद भी बिस्तर पर करवट बदलता रहता है, विश्राम रहित रहता है और उसे नींद नहीं आती। यदि वह बाह्य जगत् की चेतना भूल भी जाता है, तो भी वह सतत आ रहे स्वप्नों से परेशान रहता है। - इसका परिणाम यह होता है कि वह जैसा थका हुआ सोने जाता है, जागने पर भी वैसा ही थका हुआ रहता है। यद्यपि मन और इन्द्रियाँ इस अप्रभावी निद्रा की अवधि में थोड़ी ऊर्जा जरूर प्राप्त करती हैं; किन्तु कामना उन्हें - बलपूर्वक पुनः काम में लगा देती है। दिन-प्रति-दिन मनुष्य अपनी - नाड़ी-शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, मन तथा बुद्धि पर नियन्त्रण खोता जाता है और उसका अन्त तन्त्रिकावसाद के द्वारा या पागलखाने में होता है।
एक धनी व्यवसायी जो उसे अच्छी नींद सुला दे, उसे कुछ भी देने के लिए तैयार रहता है। एक शक्तिशाली तथा धनवान् अँगरेज को नींद नहीं आती थी। उसने सभी प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया। एक मनोचिकित्सक ने भी उसका उपचार किया; किन्तु उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु एक सामान्य मध्यमवर्गीय मनुष्य उससे आधे प्रयत्न और व्यय में ही स्वस्थ हो गया।
उपरोक्त उदाहरण यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति के पास जितनी अधिक सम्पत्ति और प्रतिष्ठित पद होगा, अनिद्रा की तीव्रता उतनी ही तीव्र होगी। जो मनुष्य पचास रुपये प्रतिमाह कमाता है, उसे एक अरबपति से अधिक सन्तोष रहता है। अरबपति को अपनी स्वयं की सुरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा और कई सौ अन्य बातों की चिन्ता रहती है। वह कामनाओं से पूर्ण रहता है। वह बहुत कम पैदल चलता है (क्योंकि वह सदा कारों में घूमता है); किन्तु वह सदा अपनी गाड़ियों पर चलता है। ऐसे व्यापारिक चुम्बकों, शक्तिशाली सम्राटों को जब तक पूर्व-संस्कारों के प्रभाव से तथा सम्पत्ति और पद से आसक्ति समाप्त नहीं हो जाती और वे कामना रहित नहीं हों जाते, कभी गहरी नींद नहीं आती।
इस पुस्तक में वर्णित विभिन्न विधियाँ बहुत सहायक हैं। अनिद्रा के बहुत से रोगियों को उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से लाभ पहुँचाया है। किन्तु ऐसे लोग जो अपने भीतर अनन्त कामनाओं और अभिलाषाओं को प्रश्रय देते हैं, वे इन नींद लाने वाली विधियों का अनुगमन करते हैं, तो उनका हाल उसी तरह रहता है जैसे एक मनुष्य धुएँ से भरे कमरे में रह कर धुएँ के कारण दम घुटने से बचने के लिए पंखे की माँग करता है। सबसे पहले कामना के कमरे से बाहर आइए, तभी आप शान्ति और प्रसन्नता की वायु में श्वास ले सकेंगे।
यदि आप अब भी न चेते, तो नाड़ी-जाल पर दबाव बढ़ जायेगा। वह व्यक्ति जो अत्यधिक तनावों में रहता है, वह यदि पागल न हो, तो भी उसे अति शीघ्र हृदय और फेफड़ों के विभिन्न रोग हो जाते हैं।
मनुष्य इन सबसे कैसे बच सकता है?
इसका एक ही उत्तर है—इच्छा रहित बनो (कामना रहित बनो)। अब देखिए, यह आपकी कैसे सहायता करता है। वह मनुष्य जिसकी कामनाएँ कम होंगी, वह शान्त होगा और इसलिए अपने कार्यों में सन्तुलित होगा। वह कामों को उनके सम्भावित परिणामों को देख कर ही हाथ में लेगा। उसके शब्द नपे-तुले होंगे। उसका मन शान्त होगा। वह कभी आवेगों के बहाव में नहीं बहता होगा। उसकी वाणी मधुर होगी। वह
इच्छा-शक्ति से निद्रा प्राप्त करना विश्वसनीय होगा। वह सभी सद्गुणों की खान होगा। याद रखें, प्रत्येक बुरे कार्य के मूल में कामना ही होती है।
ऐसा मनुष्य जिसमें कम कामनाएँ हैं, उसमें प्रचुर ऊर्जा होती है। वह असामान्य कामनाओं वाले मनुष्य से अधिक कार्य कर सकता है। कामनाओं से पूर्ण मनुष्य दिखता ऐसा है जैसे वह बहुत अधिक काम करना चाहता है; किन्तु वह सदा इधर-उधर भटकता रहता है और जो परिणाम प्राप्त होता है, उससे कई गुना अधिक उसकी नाड़ियों पर दबाव रहता है। कम इच्छाओं वाला मनुष्य चाहे धीरे-धीरे कार्य करता है, पर वह काम को शान्तिपूर्वक बिना शोर किये करता है और उसे दूसरे अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। उसकी इन्द्रियाँ उसके पूर्ण नियन्त्रण में रहती हैं। उसका मन उसका दास होता है। निष्काम मनुष्य की इन्द्रियाँ और मन सदा अन्तर्मुखी होते हैं।
ऐसे मनुष्य में मन तथा इन्द्रियाँ जब स्वाभाविक रूप से थक जाते हैं, तो वह लेट जाता है और सो जाता है। जाग्रत अवस्था में उसमें ऐसी कोई कामना नहीं होती जिसे वह धर्मानुसार पूर्ण न कर सके। इसलिए सोते समय उसके मन में कोई तीव्र इच्छा, उत्कण्ठा या अपूर्ण कामना नहीं रहती। वह रात के समय दिन के सही सदुपयोग के सन्तोष का आनन्द उठाता है तथा इस समय जीव ऊर्जा की आपूर्ति और पुनः शक्ति प्राप्त करने हेतु तथा विश्राम और शान्ति के लिए मन और इन्द्रियों को अपने भीतर समेट लेता ) है। ऐसे मनुष्य को कभी-कभी ही स्वप्न आते हैं।
मन यदि इच्छाओं का पुंज नहीं, तो कुछ भी नहीं है। इन्द्रियाँ और अन्य शारीरिक अंग भी यदि वे इच्छा के आनन्द उपभोग की वस्तुएँ या साधन नहीं हैं, तो कुछ भी नहीं हैं। जैसे-जैसे कामनाएँ घटती जाती हैं, इन्द्रियाँ अपनी बाहर भागने की प्रवृत्ति को खो देती हैं; क्योंकि वे पहचानने लगती हैं कि वास्तविक सुख अपने अन्दर ही है। मन अधिकाधिक स्वच्छ होता जाता है और अज्ञानता का आवरण पतला होता जाता है, रजोगुण और तमोगुण भी कम हो जाते हैं तथा नींद का स्तर भी परिवर्तित होता जाता है। नींद का समय भी कम हो जाता है। अब उसे संसार का ध्यान नहीं रहता; किन्तु उसमें आन्तरिक रूप से जाग्रति रहती है। ऐसे मनुष्य को नींद में चाहे वह आधे घण्टे की क्यों न हो, जिस अवर्णनीय आनन्द की अनुभूति होती है, उसमें उसके मन और इन्द्रियों को पूर्ण विश्रान्त करने की क्षमता होती है।
उच्च साधकों को बहुत कम नींद की आवश्यकता होती है; लेकिन उनकी यह अल्प निद्रा भी सामान्य मनुष्य की निद्रा से उच्च स्तर की होती है। साधक आत्मज्ञान की स्थिति में विश्राम करता है। साधक अन्दर से ईश्वर जो कि आनन्द, शक्ति और शान्ति के स्रोत हैं, उनके सम्पर्क में रहता है।
ऐसा निष्काम मनुष्य तत्क्षण गहन निद्रा में जा सकता है तथा उसके भीतर जाग्रति की ज्योति सदा जलती रहती है, इसलिए वह कभी भी इच्छानुसार जग भी सकता है। यह जाग्रति अनिद्रा के रोगी की अर्धनिद्रा से एकदम भिन्न होती है। पूर्व वाला मनुष्य पूर्णरूपेण विश्रान्त उठता है और बाद वाला मनुष्य जैसा सोने गया था वैसा ही सुस्त और थका हुआ जागता है। प्रथम वाले की नींद गहरी होती है, जब कि बाद वाले की नींद बाधित और चौकन्नी । यदि कमरे के कोने में बिल्ली भी म्याऊँ बोलती है, तो वह चौक जाता है।
महात्मा गान्धी ऐसे ही निष्काम सन्त थे जो इच्छानुसार सो और जाग सकते थे। उन्हें गहन निद्रा हेतु पाँच मिनट की अल्प अवधि पर्याप्त होती थी और वे जागने पर पूर्णतया विश्रान्त और ऊर्जावान् होते थे।
नेपोलियन बोनापार्ट भी इसीलिए विख्यात था। उसका भी अपने मन पर पूर्ण नियन्त्रण था।
आप भी यदि अपनी कामनाओं को कम करने का प्रयत्न करें, अपने मन और इन्द्रियों को अपने नियन्त्रण में लायें, तो आप भी सुखद निद्रा का आनन्द उठा सकते हैं। इन्द्रियों की स्वतः ही बाहर भागने की प्रवृत्ति होती है; क्योंकि सृष्टि-निर्माता ने उनको थोड़ा रजोगुण प्रदान किया है, किन्तु यदि आप योग-साधना के अभ्यास में यत्नपूर्वक लग जायें, तो आप उन्हें अन्तर्मुखी कर सकते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह उतना ही कठिन है जितना पहाड़ से आ रही नदी को वापस स्रोत की ओर मोड़ना । किन्तु एक शक्तिशाली जल पम्प द्वारा पानी को १००० फीट ऊँची बिल्डिंग पर चढ़ाया जा सकता है, उसी तरह आप भी जप, ध्यान और अनासक्ति योग के शक्तिशाली पम्प द्वारा इन्द्रियों के बहाव को भीतर मोड़ने में सफल होंगे।
आप सभी आध्यात्मिक धीर या आध्यात्मिक नायक बनें !
नींद के बारे में रुचिकर तथ्य
१. लकड़ी कारें, भेड़ों और सीढ़ी के डण्डों को गिनें। सोते समय गरम दूध या हार्लिक्स पियें, गन्ना चूसें,
गीता या बाइबिल पढ़ें। ये सभी आपको अच्छी नींद लाने में सहायक होंगे।
२. जब आप सोने जाते हैं, उसके ठीक पहले मस्तिष्क से रक्त वापस चला जाता है। नींद मस्तिष्क के
उस हिस्से की मृत्यु मात्र है। ३. नींद में जाने का ठीक समय बताने में कोई सक्षम नहीं है। यदि आप
यह जानते हैं कि नींद के समय मस्तिष्क में क्या होता है, तो इच्छानुसार सोना सरल होता ।
४. बच्चे गहरी नींद सोते हैं; क्योंकि वे चिन्ताओं, आकुलताओं और उत्तरदायित्वों से मुक्त रहते हैं। वे
प्रसन्नतापूर्ण रहते हैं। वे भोले और स्वच्छन्द होते हैं।
५. देश का दस में से एक प्रौढ़ व्यक्ति अनिद्रा रोग से पीड़ित है।
६. पूरी चैतन्यता के साथ विचार और निद्रा के मध्य एक अनिश्चित चेतनाशून्यता का समय होता है।
इस समय में क्या होता है तथा एकदम से चेतना चली जाती है। यह एक महान् रहस्य है। यह चिकित्सकों तथा वैज्ञानिकों के शोध, गहन अनुसन्धान तथा अध्ययन हेतु अद्भुत उदाहरण है।
७. निद्रा के समय ऊर्जा कम व्यय होती है और शरीर तथा मन नव-जीवन और विद्युत् ऊर्जा से आवेशित
हो जाता है।
८. निद्रा जीवन है। नींद का स्थानापन्न कोई नहीं है। इसके लिए न तो नशीले पदार्थ, ना ही दवाइयाँ ही
कोई सहायता कर सकती हैं।
९. निद्रा के समय रक्त के संघटक बदल जाते हैं। निद्रा के समय रक्त अधिक क्षारीय हो जाता है। यह
बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देता है। इस समय कोशिकाओं की मरम्मत शीघ्र होती है।
१०. निद्रा का श्रेष्ठ समय मध्य रात्रि से दो बजे प्रातः तक होता है।
११. निद्रा एक दैहिक परिस्थिति है जिसमें मन, मस्तिष्क और सभी अंग कुछ घड़ी विश्राम लेते हैं। नींद के
समय मन अपने उद्गम स्रोत को वापस चला जाता है ।
१२. नींद स्वस्थ जीवन हेतु प्राकृतिक बलवर्धक है। जिसे जितनी अधिक गहरी नींद आयेगी, उतना ही
अधिक वह स्वस्थ होगा।
१३. पुरुष के लिए ६ घण्टे की नींद, स्त्री के लिए ७ घण्टे की नींद तथा मूर्ख के लिए ८ घण्टे की नींद चाहिए
होती है। शिशु के लिए १० घण्टे की नींद आवश्यक है ।
१४. सोने का एक नियत समय रखें। इस समय ढीले वस्त्र पहनें। सोते समय मोटे कम्बल या मोटी चादर न
ओढ़ें।
१५. पेट के बल न सोयें। बायीं करवट सोयें। कुछ अज्ञानी जन सोचते हैं कि पेट के बल सोने से हृदय को
कोई हानि नहीं होती; किन्तु यह हृदय के लिए हानिकर है। बायीं करवट सोने से दायाँ स्वर या सूर्य
नाड़ी चलने लगती है। इससे भोजन शीघ्र पचता है; क्योंकि सूर्य नाड़ी गरम होती है।
१६. करवट ले कर सोयें, विशेषकर बायीं करवट सोयें। यह आमाशय को रिक्त करने और सूर्य नाड़ी को
चलाने में सहायक होता है।
१७. नेपोलियन बोनापार्ट मात्र चार घण्टे की नींद में विश्वास करता था। बहुत अधिक सोने से मनुष्य सुस्त
और जड़बुद्धि हो जाता है।
१८. उस कमरे में न सोयें, जिसमें खिड़कियाँ न हों।
आयुर्वेदिक उपचार
१. मृत संजीवनी सुरा
आवश्यक सामग्री--१
(१) पुराना गुड़ ८ सेर
(२) बबूल की छाल २० तोला
(३) अनार की छाल ६ माशा
(४) अडूसा की छाल ६ माशा
(५) मोचरस ६ माशा
(६) वराहक्रांता ६ माशा
(७) अतीस ६ माशा
(८) अश्वगन्धा ६ माशा
(९) देवदारु ६ माशा
(१०) बेल की छाल ६ माशा
(११) स्योनाक ६ माशा
(१२) पातल ६ माशा
(१३) सखिन ६ माशा
(१४) पिथावन ६ माशा
(१५) बड़ी कटीरी ६ माशा
(१६) छोटी कटीरी ६ माशा
(१७) गोखरू ६ माशा
(१८) बेर ६ माशा
(१९) खीरे की जड़ ६ माशा
(२०) चीते की जड़ ६ माशा
(२१) अल्कुशी के बीज ६ माशा
(२२) पुनर्नवा ६ माशा
तैयार करने की विधि
गुड़ को अलग से चूर्ण कर लें। बाकी के २१ पदार्थों को एक-साथ चूर्ण करें। इनको ३९ सेर पानी में अच्छी तरह मिलायें। इस घोल को एक ढक्कन युक्त मिट्टी के बर्तन में भरें और सोलह दिनों के लिए मिट्टी में गाड़ दें।
अब नीचे दी गयी सामग्री को तैयार करें, चूर्ण बनायें और फिर सत्रहवें (१७) दिन उपरोक्त घोल में मिलायें ।
आवश्यक सामग्री--२
(१) सुपारी १ सेर
(२) धतूरे की जड़ २ तोला
(३) लौंग २ तोला
(४) पद्माख २ तोला
(५) खस २ तोला
(६) लाल चन्दन चूर्ण २ तोला
(७) सोया २ तोला
(८) अजवाइन २ तोला
(९) गोल मिर्च २ तोला
(१०) सफेद जीरा २ तोला
(११) काला जीरा २ तोला
(१२) साठी २ तोला
(१३) जटामांसी २ तोला
(१४) दालचीनी २ तोला
(१५) छोटी इलायची २ तोला
(१६) जायफल २ तोला
(१७) मोथा २ तोला
(१८) पुनर्नवा २ तोला
(१९) सोंठ २ तोला
(२०) मेथी २ तोला
(२१) मेष श्रृंगी २ तोला
(२२) सफेद चन्दन चूर्ण २ तोला
अब मिट्टी के बर्तन को मोटे कपड़े से बाँध कर पुनः ६ दिन के लिए रख दें। सातवें दिन इसकी सुरा को निथार लें। इस सुरा सत्त्व को १ तोला ले कर २ तोला शुद्ध जल में मिलायें और रात में सोने से पहले लें। इससे अच्छी नींद आयेगी।
२. मृग मेद आसव
निम्न पदार्थों का चूर्ण बना लें:
(१) काली मिर्च २ तोला
(२) कस्तूरी ४ तोला
(३) सेंधा नमक ८ तोला
(४) जायफल ८ तोला
(५) पीपल ८ तोला
(६) दालचीनी ८ तोला
इनमें २५ तोला शुद्ध जल तथा बराबर मात्रा में पुराना शुद्ध शहद मिलायें, अच्छी तरह चलायें और इसमें मृत संजीवनी सुरा (जिसकी विधि पूर्व में बतायी गयी है) मिलायें। अब यह सारा मिश्रण जो मृत संजीवनी सुरा सहित मिट्टी के पात्र में है, इसे मिट्टी में एक माह तक गाड़ दें।
एक माह बाद इसे बाहर निकालें। तरल पदार्थ को साफ कपड़े से छान लें। यह मृगमेद आसव है। इसकी ४० बूदें डेढ़ तोला पानी में मिला कर रात भर रखें और सोने के पहले लें।
३. महाब्राह्मी तेल
आवश्यक सामग्री--१
१. चन्दन चूर्ण २० तोला
२. खस २० तोला
३. तेजपात २० तोला
४. त्रिफला २० तोला
५. सुगन्ध बाला २० तोला
६. देवदारू २० तोला
७. जटामांसी २० तोला
उपरोक्त सातों औषधियों को चूर्ण करके सात सेर पानी में तब तक उबालें, जब यह एक चौथाई बचे।
आवश्यक सामग्री--२
एक सेर सरसों के तेल को गरम करें और इसमें दो तोला हल्दी चूर्ण मिलायें ।
उपरोक्त तरल (आवश्यक पदार्थ भाग १) को गरम किये हुए सरसों के तेल में मिलायें। अब इसमें २ सेर ब्राह्मी रस (ब्राह्मी की पत्तियों के रस में) अच्छी तरह मिलायें। इस मिश्रण को तब तक उबालें, जब तक सारा पानी का अंश समाप्त न हो जाये। फिर इसमें २ सेर गाय का दूध मिलायें। अब इसे पुनः तब तक उबालें, जब तक कि पूरा दूध सूख न जाये । अब यह शेष पदार्थ महाब्राह्मी तेल है।
रात के समय इस तेल की २ तोला मात्रा अपने माथे पर लगायें और कुछ बूँदें अपने कान में डालें। इससे अच्छी गहरी नींद आयेगी।
४. बृहद्धात्री घृत
आवश्यक सामग्री--१
१. गाय का घी डेढ़ किलो
आवश्यक सामग्री- २
१. आँवले का रस डेढ़ किलो
२. सेमल की जड़ का रस डेढ़ किलो
३. बृहत कटेरी का रस डेढ़ किलो
४. वसा का रस डेढ़ किलो
५. विदारीकन्द का रस डेढ़ किलो
६. शतावरी का रस डेढ़ किलो
आवश्यक सामग्री--३
१. गज पीपली ३२ तोला
२. शीतल चीनी ३२ तोला
३. केसरी ३२ तोला
४. सफेद मूसली ३२ तोला
५. खैर की लकड़ी ३२ तोला
६. मटर ३२ तोला
७. मुद्गपर्णी ३२ तोला
८. मशपर्णी ३२ तोला
९. क्षीर काकोली ३२ तोला
१०. कोठा ३२ तोला
११. पातल ३२ तोला
१२. सहजन ३२ तोला
१३. द्राक्ष ३२ तोला
१४. अनन्तमूल ३२ तोला
१५. मकोय ३२ तोला
१६. मोथा ३२ तोला
१७. मेघनाद ३२ तोला
१८. क्षीर बिदारी ३२ तोला
औषधि तैयार करने की विधि
आवश्यक सामग्री २ के रसों को आवश्यक सामग्री १ के साथ मिला कर गरम करें। आवश्यक सामग्री ३ के पदार्थों को पीस लें और उपरोक्त उबलते हुए मिश्रण के साथ मिला दें।
उपरोक्त मिश्रण को तब तक उबालें, जब तक सामग्री २ और ३ पूर्णतया जल जायें।
अब आपको प्रथम पदार्थ घी में द्वितीय और तृतीय पदार्थों का सार प्राप्त हो जायेगा। इसे एक काँच के बर्तन या शीशी में छान लें।
इस घृत की आधा तोला मात्रा पाव-भर दूध के साथ रात को लें।
५. मस्तिष्क शक्तिवर्धक योग
यहाँ पर गहन निद्रा हेतु एक अन्य औषधि बतायी जा रही है जो भली-भाँति परीक्षित और प्रभावकारी है। यह विशेष रूप सेतन्त्रिका - दौर्बल्य प्रकार की अनिद्रा में जहाँ अनिद्रा प्रत्यक्षतः तीव्र नाड़ी-तनाव और चिन्ता तथा अपर्याप्त विश्राम के साथ अत्यधिक मानसिक श्रम के कारण होती है, ऐसे अनिद्रा रोग में उपयोगी है। यह सिर में बाहर से मालिश के लिए है। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है।
१. बादाम रोगन २ भाग
२. पोस्ता रोगन २ भाग
३. कद्दू रोगन २ भाग
४. कह रोगन २ भाग
५. ब्राह्मी तेल ८ भाग
उपरोक्त सभी पदार्थ आपको किसी पंसारी की दुकान पर मिल जायेंगे। प्रथम चारों वस्तुओं का आधा औंस तथा अन्तिम का दो औंस एक महीने के लिए पर्याप्त होगा। आधा या एक चम्मच तेल ले कर सोने के पहले सिर की मालिश कीजिए। इससे आपको अच्छी नींद आयेगी और आप उठने पर पूर्ण विश्रान्त होंगे। इस शक्तिवर्धक के नियमित प्रयोग से नाड़ियों को पूर्ण पोषण प्राप्त होता है। यह मस्तिष्क का भोजन है।
एलोपैथिक उपचार
उपचार करने से पहले यदि आप अपने मन में एक या दो बातों का विशेष ध्यान रखें, तो यह आपके लिए विशेष रूप से सहायक होगा। पहली बात तो यह है कि आप अन्य प्राकृतिक विधियों का प्रयोग करें और उनकी आपके संस्थान पर कोई प्रतिक्रिया न हो (लाभ न हो) और यदि प्राकृतिक विधियाँ प्रयुक्त करने की सुविधा न उपलब्ध हो। ये दोनों बातें हों, तो ही आप अगली बात पर जायें—वह यह है कि आपको नींद न आने का क्या कारण है या आपका अनिद्रा रोग किस प्रकार का है। नींद न आने का कारण अत्यधिक तनाव, अत्यधिक श्रम और उसके फलस्वरूप तनाव हो सकता है। यह चिन्ता के कारण भी हो सकता है। यह असामान्य नाड़ी-उत्तेजना और नाड़ियों में उच्च तनाव या हिस्टीरिया के कारण हो। सकता है या यह शारीरिक दर्द (सहने योग्य या असहनीय) के कारण हो सकता है।
ये कृत्रिम निद्रा लाने वाली या निद्राजनक औषधियाँ नाड़ी-केन्द्रों की उत्तेजनात्मकता को दबा कर या केन्द्र पर पहुँचने वाले प्रभावों के संचालन को जहाँ वे संवेदक अंगों पर प्रभाव डालते हैं, वहाँ या कि उनके उद्गम-स्थान पर रोक कर मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करती हैं।
अनिद्रा हेतु अत्यन्त प्रभावकारी बहुत-सी औषधियाँ उपलब्ध हैं। आप रोग तथा अपनी प्रकति के अनुरूप औषधि का चुनाव कर सकते हैं। बतायी गयी निम्न औषधियों को अपने विवेक के अनुसार प्रयोग करें:
क्लोरल हाइड्रेट, ब्रोमाइड्स, पैरडिहाइड, सल्फोनल (मेथिलसल्फोन और टेट्रोनल, ये भी इसी समूह में आती हैं), बारबीटोन्स (इसे वेरोनल भी कहते हैं), यूरेथ्रेन (यह कुछ पेटेंट औषधियों जैसे यूफोरिन, हेडोनल, एडेलिन, यूरेडल, फ्रोपोनल, ब्रोम्यूरल, फीनोबारबीटोन, ल्यूमिनल आदि के रूप में उपलब्ध है)।
सल्फोनल-समूह सरल अनिद्रा रोग में उपयोगी है; किन्तु यह जब दर्द अथवा नाड़ियों में उत्तेजना हो, तो अनुपयोगी है। यह हृदय पर कोई हानिकर प्रभाव नहीं डालती ।
सम्पूर्ण यूरेथ्रेन-समूह जैसे बारबीटोन नाड़ी-सम्बन्धी अनिद्रा रोग में बहुत उपयोगी है। बारबीटोन या वेरोनल, सल्फोनल से अधिक तीव्र है और उसके समान ही सुरक्षित भी है। मन्दबुद्धि के अनिद्रा रोगी तथा हिस्टीरिया के रोगियों में इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। यूरेथ्रेन औषधियाँ धीरे-धीरे असर दिखाती हैं, फिर भी वे सुरक्षित हैं, इसलिए वे पुनः की जा सकती हैं। एडेलिन से मीठी और प्राकृतिक नींद आती है।
कुछ लोगों को ल्यूमिनल गोलियाँ भी अनुकूल होती हैं। चूँकि ये हृदय पर कोई हानिकर प्रभाव नहीं डालतीं, इसलिए हृदय रोग से होने वाले अनिद्रा रोग के लिए अच्छी हैं। वे बच्चों को भी अनुकूल होती हैं। तन्त्रिकावसाद के अनिद्रा रोग में हीडोनल लाभकारी पायी गयी है। यह हिस्टीरिया से पीड़ित स्त्रियों में भी लाभदायक है। ल्यूमिनल नाड़ी-उत्तेजना की स्थिति, सहने योग्य दर्द, मतिभ्रम, मनोवैज्ञानिक कष्ट, उन्माद, भ्रम आदि में उपयोगी है। बच्चों के लिए टेट्रोनल और ट्रायोनल भी प्रयोग किये जाते हैं। इनको कुछ गरम पेय जैसे सूप अथवा दूध के साथ घोल कर देना अधिक अच्छा होगा। चूँकि ये धीरे-धीरे असर करते हैं, इसलिए इन्हें सोने के तीन या चार घण्टे पहले दिया जाना चाहिए।
चिन्ता, अत्यधिक श्रम तथा वृद्धावस्था से होने वाले अनिद्रा रोग में क्लोरल हाइड्रेट, इसके विभिन्न रूप जैसे सीरप क्लोरल तथा डोर्मिटाल आदि सबसे सरल, सुरक्षित और श्रेष्ठ निद्राजनक औषधि हैं। इससे विश्रान्तिपूर्ण निद्रा आती है। यह मस्तिष्क के मुख्य केन्द्रों की उत्तेजनात्मकता को कम करके काम करती है। ब्यूटिल क्लोरल जो क्लोरेटोन के रूप में उपलब्ध है, वह भी इसी प्रकार कार्य करता है।
किसी भी अनिद्रा रोग में, रोग की तीव्रता में चिकित्सक की सलाह और निर्देश के बिना निद्राजनक कोई भी औषधि न दें।
अनिद्रा रोग के लिए होमियोपैथिक औषधियाँ
१. सिनिफ्यूगा रेसीमोसा :जब मस्तिष्क में उत्तेजना के लक्षण के साथ अनिद्रा रोग हो। यह
नाड़ी-संस्थान, पेशी-संस्थान, गर्भाशय और अण्डाशय पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इस कारण यह आवश्यक रूप से स्त्री औषधि है। यह बच्चों में दाँत निकलते समय मस्तिष्क में उत्तेजना के कारण नींद न आने में उपयोगी है। मात्रा—३ शक्ति ।
२. काफिया क्रूडा : जब व्यक्ति लम्बा, पतला और आगे की ओर झुका हुआ हो, उसका रंग गहरा और
क्रोधी स्वभाव का हो, तभी काफिया क्रूडा के बारे में विचार करें। जब अनिद्रा के साथ मन और शरीर की असामान्य गतिविधि या आकस्मिक भावनात्मक व्याकुलता हो, तो काफिया क्रूडा निर्देशित की जाती है। मात्रा - ३ से २०० शक्ति ।
३. सायप्रीपेडियम : यह विशेष रूप से बच्चों को अनुकूल होती है। बच्चा रात में रोता है। वह रात को
जागता है और प्रसन्न रहता है, खेलता रहता है। मात्रा — अर्क को ६ भाग पतला करके दें।
४. डफ्ने इंडिका : जब नींद न आने के साथ-साथ हल्का दर्द जो शीघ्रता से चला जाता हो, हड्डियों में
दर्द और रात में चौंकाने वाले स्वप्न आते हैं, तब डपने इंडिका निर्देशित की जाती है। आप डफ्ने इंडिका के रोगी को इस लक्षण से भी पहचान सकते हैं कि उसकी जीभ पर एक तरफ जमाव रहता है। मात्रा -१ से ६ शक्ति ।
५. जेल्सेमियम : यहाँ प्रतिक्रिया अधिकतर नाड़ी-संस्थान पर होती है। यदि अत्यधिक तथा
अनियन्त्रित चिन्तन या थकावट के कारण नींद न आ रही हो, तो जेल्सेमियम का प्रयोग करना चाहिए।
६. इग्नेटिया : यह हिस्टीरिया से पीड़ित रोगियों के लिए है। जब रोगी सोने जाता है, तो उसके अंगों
में झटका लगता है। नींद न आने का मुख्य कारण दुःख, देखभाल, चिन्ता और व्याकुलता होता है। रोगी की बाँहों में खुजली होती है और वह बहुत अधिक उकताया हुआ रहता है। रोगी को कभी अच्छी नींद नहीं आती। निरन्तर चल रहे स्वप्नों से वह परेशान रहता है। यह मुख्यतया स्त्री औषधि है। मात्रा—६ २०० शक्ति ।
७. ह्योस्सायामस हाइड्रोब्रोमाइड : तीव्र अनिद्रा रोग, विशेषकर ऐसे लोगों जो झगड़ालू, उन्मादी और अश्लील
चरित्र वाले होते हैं, को ह्योस्सायामस हाइड्रोब्रोमाइड दिया जाता है। ऐसे रोग में रोगी नींद में चौक जाता है। मात्रा – ६ से २०० शक्ति ।
८. पैसीफ्लोरा इनकारनाटा : इस रोग में मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं पड़ता; किन्तु वहाँ थकावट के कारण विश्राम
नहीं मिलता और रोगी जागता रहता है। यह विशेष रूप से दुर्बल, नवजात शिशुओं और वृद्ध लोगों को दी जाती है। मात्रा अर्क को ही बड़ी मात्रा में प्रयोग करें—३० से ६० बूँद और अक्सर पुनरावृत्ति करें ।
९. सेलेनियम : सभी रक्तवाहिनियों में विशेष रूप से उदर-क्षेत्र में धड़कन होने पर सेलेनियम
निर्देशित की जाती है। रोगी को सामान्यतया अर्धरात्रि तक नींद नहीं आती और वह प्रातः जल्दी जाग जाता है और सदा एक ही समय जागता है। सेलेनियम के रोगी में बहुत अधिक अशक्तता होती है। मात्रा - ६ से ३० शक्ति ।
१०. सिलीसिया : इसमें रोगी को प्रबल उत्तेजना और सिर में गरमी के कारण नींद नहीं आती। वह
नींद में एकदम से चौंक जाता है। उसे नींद में बुरे स्वप्न बाधा उत्पन्न करते हैं। सिलीसिया के रोगी दोषपूर्ण अभिशोषण और कुपोषण का शिकार होते हैं। मात्रा—६ से ३० शक्ति ।
११. चामोमिला : यह मुख्यतया बच्चों की औषधि है। बच्चा ठीक से सो नहीं पाता, वह निद्रित रहता
है, वह सिसकता है, वह नींद में रोता और विलाप करता है। वह बुरे स्वप्नों के कारण अचानक भयभीत हो जाता है। जब बच्चा सोता है, तो उसकी आँखें आधी खुली रहती हैं। मात्रा - १२ से ३० शक्ति ।
१२. नक्सवामिका : यह आधुनिक फैशनेबल जीवन की स्थितियों के कारण होने वाले अनिद्रा रोग के
लिए है। नक्सवामिका को तब देना चाहिए, जब नींद न आने का कारण अधिक अध्ययन, चिन्तन या पढ़ाई हो, यदि रोगी आरामदेह जीवन व्यतीत करता है या उसे पाचन सम्बन्धी विकार रहते हैं। नक्सवामिका का रोगी सुबह तीन बजे के बाद प्रातः तक नहीं सो पाता। उसे पर्याप्त निद्रा नहीं आती; इसलिए वह जागने पर थका हुआ अनुभव करता है। वह भोजन के तुरन्त बाद और शाम को भी सोना चाहता है। वह यदि बाधा न डाली जाये, तो थोड़ी झपकी के बाद सदा अच्छा अनुभव करता है। मात्रा -१ से ३० शक्ति शाम के समय दें।
१३. ओपियम : ओपियम के रोगी का मुख्य लक्षण यह है कि वह निद्रालु होता है, वह सोना चाहता है;
पर सो नहीं पाता। उसकी नींद स्वप्नों और दूर की आवाजों से बाधित रहती है। मात्रा—३ से ३० शक्ति तथा २०० शक्ति भी ।
१४. पल्सेटिला : इसके रोगी में पेट की कुछ खराबी रहती है। रोगी दोपहर में सोना चाहता है; किन्तु
वह शाम को देर तक जागता रहता है। यह मुख्यतया स्त्री औषधि है। वह अपने मस्तक पर हाथ रख कर सोती है। मात्रा—६ से ३० शक्ति ।
बायोकेमिक उपचार
बायोकेमिक उपचार पद्धति के अनुसार अनिद्रा मस्तिष्क और नाड़ी - संस्थान में खनिज लवणों के असन्तुलन से उत्पन्न होती है। बायोकेमिक औषधि उस कमी की पूर्ति करके उस सन्तुलन को पुनः लाती है और इस प्रकार यह मस्तिष्क और नाड़ियों की सामान्य क्रियाविधि प्रारम्भ करती है।
मस्तिष्क और नाड़ियों के कार्यों की दो असामान्य स्थितियाँ होती हैं— चिन्ता, अत्यधिक श्रम और मस्तिष्क को रक्त का बहुत अधिक प्रवाह तथा मस्तिष्क से इसका निकास न होना। इन सभी कारणों से अनिद्रा या जागते रहने की स्थिति उत्पन्न होती है। मस्तिष्क और नाड़ियों के थकने के परिणामस्वरूप सुस्ती या निद्रालुता होती है; किन्तु अच्छी नींद नहीं आती। दोनों ही विषयों में बायोकेमिक औषधियाँ प्राकृतिक अवस्था को पुनः लाती हैं।
१. फेरम फास : यहाँ रोग का कारण ज्वर होता है। विभिन्न भागों में रक्त का जमाव रोगी को जगाये रखता
है। विश्राम का अभाव ही इसका लक्षण है ।
२. काली फास : यह बायोकेमिक औषधियों में सबसे आगे है। यह प्रथम श्रेणी का नाड़ी - लवण है। जब
उत्तेजना, चिन्ता, व्याकुलता, व्यापार या घरेलू कठिनाइयों के कारण नींद न आती हो, या कि उसका कारण अति-परिश्रम या दुःख हो, तब काली फास निर्देशित की जाती है। रोगी विश्राम - रहित रहता है, वह स्वयं को ढीला छोड़ देता है और उबासी लेता है। वह निद्रालु रहता है। बच्चे जो नींद न आने से सोते समय रोते और सिसकते हैं। ऐसे सभी रोगियों को काली फास दी जाती है।
३. मैग्नेशिया फास :इसमें नींद न आने का कारण कमजोरी रहता है। मैग्नेशिया फास के रोगी को मस्तिष्क पर
दबाव का विचित्र अनुभव होता है जैसे वह सिकुड़ा हुआ हो । इस लक्षण द्वारा आप उसे पहचान सकते हैं।
४. नेट्रम मूर : रोगी रात में सोता है; किन्तु फिर भी वह जागने पर पूर्ण विश्रान्त नहीं रहता। उसे सतत सोने
की इच्छा रहती है। उसे सुबह भी सोने की इच्छा रहती है। नेट्रम मूर के रोगी के मुँह में से सोते समय लार गिरती है।
५. नेट्रम सल्फ : इसका रोगी भी सुस्ती और निद्रालुता का अनुभव करता है। उसकी जीभ का परीक्षण कीजिए।
यदि आप देखें कि जीभ पर भूरा या स्लेटी जमाव है, तो नेट्रम सल्फ दीजिए। रोगी के मुँह का स्वाद कड़वा रहता है और सुस्ती के साथ पैत्तिक लक्षण रहते हैं।
मात्रा— पाँच गोलियाँ प्रत्येक एक या दो घण्टे में लें। जैसे-जैसे स्थिति सुधरती जाये, दवाई की मात्रा
कम करते जायें।
प्राकृतिक उपचार
नींद एक आयुर्वर्धक रसायन है। यह एक शक्तिशाली मल्हम है। यह दिन में व्यय हुई ऊर्जा को पुनः भरती है। एक मनुष्य जो रात में गहरी नींद सोता है, वह जागने पर पूर्ण विश्रान्त रहता है और ऊर्जावान् भी होता है। वह मनुष्य जो बहुत दिनों से सोया नहीं होता, वह मानसिक असन्तुलनों का शिकार हो जाता है। यह जड़ और चेतन सभी के लिए आवश्यक है। जड़ वस्तुओं जैसे औजारों और मशीनों में इसे 'Fatigue' कहते हैं, जो कि विश्राम द्वारा दूर की जा सकती है। यहाँ तक कि जड़ मशीनों को भी विश्राम की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे लम्बे समय तक काम नहीं कर सकेंगी।
दिन और रात की ही तरह काम और निद्रा बहुत आवश्यक हैं। रात १० बजे से प्रातः ४ बजे तक का समय नींद का सर्वश्रेष्ठ समय है। नींद न आना एक रोग है। यह शरीर की वृद्धि को रोक देती है और बहुत से रोगों का कारण होती है। वह मनुष्य जो अच्छी नींद सोता है और उचित मात्रा में काम करता है, उसका मन और शरीर स्वस्थ रहता है। अत्यधिक श्रम और अपर्याप्त निद्रा मन सन्तुलन को बिगाड़ देती हैं जिससे शीघ्र ही शरीर कमजोर हो जाता है और आवश्यक कार्य हेतु अयोग्य हो जाता है। कारण और प्रभाव का सिद्धान्त संसार में सभी जगह काम करता है। अनिद्रा के मूल में भी कुछ कारण हैं।
अनिद्रा या नींद न आने के कारण
इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कारण है चिन्ता; इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि चिन्ता कम करें और काम अधिक। चिन्ताएँ मन की शान्ति में विघ्न डालती हैं और नींद न आने का कारण होती हैं।
दूसरा कारण है अत्यधिक परिश्रम। जितना सम्भव हो, इससे बचें। अत्यधिक काम करने से मन का सन्तुलन बिगड़ जाता है। जब काम का समय हो, तब काम करें। जब सोने का समय हो, तब सोयें। यह स्वस्थ रहने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए रात १० बजे के बाद जहाँ तक सम्भव हो, काम न करें।
तीसरा कारण है अनियमित आदतें। इसलिए इनसे बचें। सभी विषयों में नियमितता —यही शरीर को स्वस्थ और फुरतीला बनाये रखने की कुंजी है।
चौथा कारण है सोने हेतु जाने के पूर्व विषय-सुख या इन्द्रिय-सुख देने वाले विचार रखना। सोने हेतु जाने से पहले धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना अति-आवश्यक है।
किसी कारण से सिर में अत्यधिक गरमी होने से भी नींद में विघ्न पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहते है कि 'पैर गरम रखना चाहिए और सिर ठण्ढा ।'
शारीरिक रोग जैसे कब्ज, ज्वर और अन्य रोग भी गहरी नींद में बाधा डालते हैं। शरीर और मन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। प्रकृति अत्यन्त कठोर न्यायाधीश है; इसलिए यह हठी और नियमों के प्रतिकूल चलने वालों को सहन नहीं करती । अतः स्वास्थ्य के नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें।
यदि शरीर स्वस्थ होगा, तो नींद से सम्बन्धित कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे दिन के बाद रात आती है, उसी तरह वह स्वयं अपने-आप आयेगी। सबसे अनिवार्य बात यह है कि आप स्वास्थ्य के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन कर शरीर को स्वस्थ रखें।
सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि शौच नियमित और मुक्त रूप से हो। पाचन अच्छा होना चाहिए, जिससे कब्ज न होने पाये। यदि आप थोड़े भी कब्ज का अनुभव करें, तो तुरन्त एनिमा लें। कब्ज एक हजार एक रोगों की जड़ है; इसलिए हमें कब्ज के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए और उसे शीघ्र दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ।
अनिद्रा से बचने हेतु निम्न सावधानियाँ रखें
१. सोने जाने से पहले भारी भोजन न लें।
२. सोने जाने से पूर्व किसी गम्भीर विषय पर विचार न करें।
३. रात को देर तक न जागें ।
४. सिनेमा देखने न जायें ।
५. अपनी आँखों पर जोर न डालें।
अच्छी नींद लाने हेतु उपाय
१. अपना रात का भोजन ७ बजे शाम से पहले समाप्त कर दें। यह हल्का होना चाहिए।
२. शाम के भोजन में दूध और फल या छाछ और सस्ते फल लेना अधिक अच्छा होगा।
३. सोने जाने से पहले नियमित रूप से धार्मिक पुस्तकें कम-से-कम आधा घण्टे अवश्य पढ़ें।
४. यदि आपके पास समय और ऊर्जा हो, तो रात को ९ बजे से ९.३० बजे तक एक मील पैदल भ्रमण करें।
५. गरमी के मौसम में आप सोने जाने के पहले ठण्डे पानी से स्नान कर लें। ठण्ढ के मौसम में गरम पानी
से नहायें। यदि आप ऐसा न कर सकें, तो सोने के लिए जाने से पहले एक गिलास गरम पानी या दूध पियें।
६. अपनी आँखों और मस्तक पर ठण्डे पानी की पट्टी रखें। अच्छी नींद की प्राप्ति हेतु ये प्राकृतिक साधन
हैं।
७. आयुर्वेदिक औषधि हेतु आप माथे पर चन्दन और कपूर का लेप लगा सकते हैं।
८. आप बायोकेमिक औषधि 'काली फास' का प्रयोग कर सकते हैं।
९. यदि सम्भव हो, आप तुलसी की चाय ले सकते हैं।
१०. आप कुछ मिनट तक शवासन कर सकते हैं।
११. अन्त में इष्टमन्त्र का जप करें। ईश्वर में पूर्ण आस्था रखें। वे सदा सभी पर दया करते हैं। वे उनकी
सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं।
सामान्य ज्ञान द्वारा उपचार
यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और आपका पक्का विश्वास है कि इस संसार से परे स्वर्ग है और आप बाद में वहाँ जाने की अभिलाषा रखते हैं, तो आप अपने भाव के अनुसार स्वर्ग के बारे में विचार करें। एक ऐसी सीढ़ी की कल्पना करें जो इस संसार को स्वर्ग से जोड़ती है। अब आप उस सीढ़ी के डण्डों पर एक के बाद एक करके चढ़ते जायें। आप जानते ही हैं कि कई मील लम्बा क्षेत्र है जो इस जगत् को स्वर्ग से अलग करता है; इसलिए आपकी सीढ़ी में अरबों-खरबों डण्डे होंगे। किन्तु आप किसी भी प्रकार स्वर्ग में पहुँचना चाहते हैं। इसलिए सीढ़ी पर चढ़ना जारी रखिए। अपना ध्यान इस काम में लगाइए। अपनी पलकें बन्द रखिए। उन्हें खोलिए मत। आप शीघ्र ही निद्रा में लीन हो जायेंगे।
या, शायद आपके पास कोई पालतू पशु-कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या भेड़ होगी। तब आप सोचें कि आप एक बहुत बड़े पशुपालक हैं। आप अपने पशुओं को बाहर चराने ले गये हैं। उन्हें अपने बाड़े में लाने के पहले आप यह पक्का करना चाहते हैं कि सभी पशु सुरक्षित वापस आ गये हैं या नहीं। उनकी गिनती करना प्रारम्भ कीजिए। पहले एक को बाड़े में जाने दीजिए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को — इसी प्रकार गिनते जाइए, जब तक आप नींद में न चले जायें।
यदि आप सेना के अधिकारी हैं, तो भेड़ के स्थान पर आपके पास बहुत से सैनिक होंगे और आप उनकी गिनती करते-करते सो जायेंगे ।
यदि आप एक व्यापारी हैं, तो आप कपड़ों के थान या शक्कर या चावल की बोरी गिन सकते हैं। मानसिक रूप से उन्हें अपने गोदाम से बाहर राह देख रहे हजारों ग्राहकों को दीजिए। उन ग्राहकों को एक-एक करके निपटाते जाइए, जब तक कि आप उन्हें गिनने में असमर्थ न हो जायें और आप गहरी निद्रा में चले जायेंगे। यदि आप एक कैशियर हैं, तो एक हजार रुपयों को सिक्कों में गिनिए, जिनमें में ढेर सारे एक रुपये के सिक्के हैं और सभी प्रकार के सिक्के हैं।
यदि आप एक स्कूल मास्टर या प्रोफेसर हैं, तो आप उपरोक्त सबके स्थान पर बहुत से विद्यार्थी ले सकते हैं और उन्हें उपाधि-पत्र बाँटिए। आप एक अत्यन्त लोकप्रिय व्याख्याता हैं; इसलिए आपके पास हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आपको सोने के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी मिल जायेंगे ।
किन्तु मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा नींद लाने का नुस्खा बताता हूँ। अपनी इतिहास या भूगोल की पुस्तक ले लें (मैंने सोचा कि आपको ये विषय पसन्द नहीं होंगे, इसलिये मैंने ये विषय बताये हैं; किन्तु अगर आप इतिहास-भूगोल में अच्छे हैं, तो गणित की पुस्तक लीजिए या अन्य कोई विषय जो आपको अच्छा न लगता हो और जिसे आप परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ते हों ! । अब उसे पढ़ते जायें।
दृढ़ रहें। स्वयं से कहें — “मैं इस समय और कोई पुस्तक नहीं पढूँगा।” आप पायेंगे कि लैंप सारी रात जलता रहा। आप जहाँ थे, वहीँ सो गये - पुस्तक के तीसरे पन्ने पर ही ।
आध्यात्मिक साधकों (जिन्हें वेदान्तिक पुस्तक पढ़ने में अधिक रुचि नहीं होती) को कोई बड़ी वेदान्त की पुस्तक ले लेनी चाहिए, जिसमें बड़े-बड़े वाक्य और कठिन शब्द हों और उसको पढ़ना प्रारम्भ कर देना चाहिए ।
किन्तु अधिकांश आध्यात्मिक साधकों को जप माला ही मीठी लोरी का काम करती है। सारे बल्ब या ट्यूब लाइटें चालू कर दें। बिस्तर पर बैठ जायें। मोटी चादर या कम्बल ओढ़ लें। माला ले लें और थोड़ी देर जप करें (आपको आश्चर्य होगा कि इससे थोड़ी देर में क्या होगा ?) बाद में आप पूरी तरह बिस्तर में लेट कर जप करेंगे और आपको चार बजे के एलार्म की आवाज सुनायी देगी।
मान लीजिए, जप के कारण आप जागते रहते हैं, तो और भी अच्छा है। तब आप सोइए नहीं, भगवन्नाम का जप करते जाइए। आपको अति शीघ्र नींद नहीं, समाधि प्राप्त होगी। भगवान् ऐसे साधक को अपना आशीर्वाद प्रदान करें !
अपने बिस्तर का स्थान जल्दी-जल्दी न बदलें। यदि आप एक ही प्रकार के बिस्तर पर, एक ही कमरे में, एक ही समय पर, एक ही स्थिति में सोयेंगे, तो आपको शीघ्र नींद आयेगी। जिस मनुष्य को कड़े गद्दे पर सोने की आदत होती है, उसे स्प्रिंगदार गद्दे पर सोने में कष्ट होता है, इसके विपरीत जो मनुष्य चौड़े बिस्तर पर या भूमि पर सोने का आदी होता है, उसे सँकरे बिस्तर अथवा खटिया पर नींद नहीं आती।
क्या आपने प्रकृति की इस आश्चर्यजनक रचना पर कभी ध्यान दिया? जो जितना अधिक बुद्धिमान् प्राणी है, वह उतना ही सीधा या लम्बवत् है। जिन प्राणियों में किंचित् मात्र भी बुद्धि नहीं है, वे पूरी तरह भूमि के समानान्तर हैं।
जिनमें बहुत थोड़ी बुद्धि है, उनका सिर रीढ़ के ऊपर स्थित है। एक बन्दर जो सदा उछल-कूद करता रहता है, वह भूमि के समानान्तर चलता है। और अपना सिर ऊपर उठाये रखता है और लम्बवत् बैठता है। और मनुष्य जो महान् विचार-शक्ति का धनी है, वह सदा सीधा रहता है और भूमि पर समानान्तर लेटने में असुविधा का अनुभव करता है। माँ प्रकृति ने ऐसी रचना इसलिए की है, ताकि मस्तिष्क में बहुत कम रक्त एकत्र हो सके। इसके बाद भी मूर्ख मनुष्य अनगिनत कामनाओं से प्रेरित हो कर बहुत अधिक सोचता है और अनिद्रा से पीड़ित होता है। हे मानव, अपने हृदय में निवास करने वाले ईश्वर का ध्यान करो। विचार करना बन्द करो। आपके मन और बुद्धि शान्त हो जायेंगे।
नामोपचार
महामृत्युंजय-मन्त्र
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ।।
अर्थ
हम त्रिनेत्रधारी (भगवान् शिव) की आराधना करते हैं, जो सुगन्धित हैं और जो सभी प्राणियों का भली प्रकार पोषण करते हैं। वे हमें मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें जिससे हम अमरत्व को प्राप्त कर सकें, उसी प्रकार जैसे एक कद्दू उसके बन्धन (लता) से टूट कर अलग हो जाता है।
लाभ
१. यह महामृत्युंजय-मन्त्र जीवन-रक्षक मन्त्र है। इन दिनों, जब कि जीवन बहुत जटिल है, दुर्घटनाएँ
प्रतिदिन होती रहती हैं, यह मन्त्र सर्पदंश, बिजली गिरना, मोटर दुर्घटनाओं, अग्नि दुर्घटनाओं, साइकिल दुर्घटनाओं, जल दुर्घटनाओं तथा अन्य सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में हमें मृत्यु से से बचाता है। इनके साथ ही इसमें महान् आरोग्यकर प्रभाव भी है। वे रोग जो चिकित्सकों द्वारा असाध्य घोषित कर दिये जाते हैं, वे भी जब इस मन्त्र को शुद्ध हृदय, पूर्ण विश्वास और निष्ठापूर्वक जपा जाता है, तो ठीक हो जाते हैं। यह समस्त रोगों के विरुद्ध अस्त्र है। सारांश में यह मृत्यु पर विजय पाने का मन्त्र है। आप सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जायेंगे।
२. यह मोक्ष-मन्त्र भी है। यह शिव भगवान् का मन्त्र है। यह हर दीर्घायुष्य, शान्ति, ऐश्वर्य, पुष्टि, तुष्टि
और मोक्ष प्रदान करता है।
३. अपने जन्म-दिन पर इस मन्त्र का एक लाख या कम-से-कम पचास हजार मन्त्र-जप करें, हवन करें
और साधुओं, निर्धनों तथा बीमारों को भोजन करायें। यह आपको दीर्घायु, शान्ति और समृद्धि प्रदान करेगा। हरि ॐ तत् सत् ।
नीचे बताये उपायों को करें : आप अच्छी नीद सोयेंगे
१. कोई भी निद्रा लाने वाली औषधि न लें ।
२. सोने से पहले गरम पानी से स्नान करें।
३. सोने के ठीक पहले कुछ हल्का और स्फूर्तिदायक तरल पेय जैसे दूध, कोको या हार्लिक्स पीना चाहिए।
यह रक्त को मस्तिष्क की ओर भागने से रोक कर उसे आमाशय की ओर भेजता है।
४. यह ध्यान रखें, सोने का कमरा भली-भाँति संवाती हो (अर्थात् जिसमें हवा का आवागमन अच्छी तरह
हो) ।
५. सोने के लिए सख्त बिस्तर का प्रयोग करें।
६. हल्के किन्तु गरम चादर या कम्बल का ओढ़ने हेतु प्रयोग करें।
७. सोते समय कसे हुए कपड़े न पहनें।
८. दिन के समय, विशेषकर शाम को, कोई भी उत्तेजक पदार्थ न लें। चाय, काफी, उत्तेजना लाने वाले
भोज्य पदार्थ त्याग दें।
९. यदि आप मानसिक या बुद्धि के काम करते हैं, तो आपको काफी व्यायाम करना चाहिए। प्रात: और
सायंकाल तेजी से लम्बी दूरी तक पैदल भ्रमण करने से आपको विश्राम से पूर्ण विश्रान्तिदायक निद्रा आयेगी।
१०. धूप में बैठें और सूर्य को अपनी ऊर्जावान् किरणों का आशीर्वाद आपको प्रदान करने दें।
११. यदि आप मस्तिष्क में रक्त के अधिक प्रवाह से निरन्तर पीड़ित हैं, • आप थोड़ा मोटा तकिया प्रयोग
करें। अपने सिर को थोड़ा अधिक उठा कर रखें।
१२. बायीं करवट सोयें—यह योगियों की विधि है। इससे पिंगला नाड़ी चलने लगेगी और आपको
विश्रान्तिपूर्ण निद्रा प्रदान करेगी।
१३. सोने के ठीक पहले एक घण्टे जप और ध्यान करना सभी शक्तिवर्धकों से श्रेष्ठ है। आप जब सोने
जायें, आपका मन सात्त्विक होना चाहिए। इससे आप नींद में प्रचुर ऊर्जा ग्रहण करेंगे।
१४. यदि आपको नींद न आ रही हो, तो चिन्ता न करें। भगवान् का नाम जपें। इस अनिद्रा का अपने श्रेष्ठ
आध्यात्मिक लाभ हेतु उपयोग करें। असामान्य स्थिति चली जायेगी।
१५. सोने से पहले चुकन्दर की कुछ पत्तियाँ चबायें ।
१६. सोने जाने से पहले कुम्भकर्ण और मुचुकुन्द को याद करें। जो बहुत गहरी नींद सोते हैं, उनमें ये दोनों
सर्वश्रेष्ठ हैं।
मन्त्रों से रोग का उपचार
बहुत बार कुछ शारीरिक रोग हमारी नींद में विघ्न डालते हैं। इस रोग को दूर करने के लिए अच्छी नींद आना भी आवश्यक है। औषधि द्वारा उपचार के साथ-साथ श्री स्वामी जी महाराज रोगी को हमेशा नामोपचार तथा प्रार्थना द्वारा उपचार की सलाह भी देते थे।
प्राणिक और मन्त्रों द्वारा उपचार के विषय में भी श्री स्वामी जी महाराज स्वयं की ही विशिष्ट विधि प्रयोग करते थे। उनका लक्ष्य रोग का उपचार करने वाले और जिनका उपचार किया जा रहा है; मात्र रोग ठीक करना ही नहीं, वरन् उनका स्थायी आध्यात्मिक कल्याण करना था। स्वामी जी की विधि वशीकरण के स्थान पर प्रार्थना थी। यह इस सत्य को स्वीकार करने पर आधारित थी कि रोग को ठीक करने वाला ईश्वर है और यह कि जो लोग रोग ठीक करना चाहते हैं, वे स्वयं तथा रोगी—दोनों को ही ईश्वर के साथ लय में होना चाहिए। जो पत्र नीचे दिया गया है, वह श्री स्वामी जी ने अपने भक्त को लिखा था जो स्वयं ही ईश्वर प्रदत्त रोगहरण की शक्ति से सम्पन्न था और उसने इस शक्ति में यम-नियम, जप, ध्यान और कीर्तन के अभ्यास द्वारा बहुत वृद्धि कर ली थी और उसमें इसके प्रति गहन रुचि थी।
-प्रकाशक
प्रिय आत्मन्,
प्रणाम और नमस्कार! ॐ नमो नारायणाय ।
जैसा आपने चाहा था, मैं मन्त्र की सहायता से रोग के उपचार की पद्धति का विस्तृत विवरण नीचे दे रहा हूँ।
इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण बिन्दु जो सदा याद रखना चाहिए, वह यह तथ्य है कि वह सर्वशक्तिमान् ईश्वर है जो रोगी को स्वस्थ करता है, न कि हमारी संकल्प-शक्ति। हमारा कर्तव्य है कि हम उस ईश्वर से इच्छा-शक्ति तथा रोगहरण हेतु प्रार्थना करें और रोगी के मन को उस सर्वव्यापक संकल्प-शक्ति के साथ-साथ जप, कीर्तन आदि के द्वारा एक लय में लाने का प्रयास करें। प्रार्थना दोनों की कुंजी है।
कृपा करके एक छोटा सत्संग आयोजित करें। वह व्यक्ति जिसका उपचार करना है, उसे भी वहाँ होना चाहिए। जितने अधिक-से-अधिक उच्च साधक और भक्त मिलें, उन सभी को भी वहाँ होना चाहिए। सभी को यह बताना आवश्यक नहीं है कि यह सत्संग उपचार हेतु आयोजित है। उनकी सम्मिलित प्रार्थना का बल रोगी के लिए महान् सहायक होगा।
ॐ के उच्चारण, गणेश और गुरु-कीर्तन से प्रारम्भ कीजिए। श्री हनुमान् जी की स्तुति कीजिए और दस से पन्दरह मिनट महामन्त्र कीर्तन कीजिए। यदि सम्भव हो, तो (यदि रोगी रोग की गम्भीरता के कारण लेटा हुआ न हो) रोगी भी कीर्तन करे। किसी भी विषय में रोगी (स्त्री या पुरुष) को पूर्ण विश्राम करने दें और जितना सम्भव हो, उसे ईश्वर तथा उनकी रोगहरण हेतु कृपा पर पूर्ण आस्था रखते हुए ईश्वर के बारे में सोचने के लिए कहें।
जब थोड़ी एकाग्रता आपके भीतर आ जाये, तब आप ईश्वर से रोगी पर अपनी कृपा-वृष्टि तथा आशीर्वाद देने हेतु प्रार्थना करें। इसके बाद महामृत्युंजय- -मन्त्र का जप प्रारम्भ करें। थोड़ी देर तक मन्त्र को जोर से बोलें, फिर कुछ मिनट तक मानसिक जप करें। सारे समय यह भावना करें कि ईश्वर की कृपा से रोगी स्वस्थ हो रहा है। रोगी को भी यह अनुभव करना चाहिए कि मन्त्र की महान् शक्ति उसके चारों ओर फैली हुई है। वह उसकी रक्षा कर रही है।
इसके बाद शान्ति-मन्त्र : “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः! असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृत गमय ।। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः !"
अब कुछ मिनट तक यह अनुभव करते हुए कि ईश्वर की कृपा रोगी में आपूरित हो गयी है, ध्यान करें और यह सम्पूर्ण क्रियाविधि उसे अर्पित कर दें और उठ जायें।
उपरोक्त कार्यक्रम की समाप्ति पर रोगी एक दृढ़ मानसिक भावना के साथ कि वह ईश्वर की इच्छा से ठीक हो गया है, विभूति का प्रसाद दें।
भगवान् आप पर कृपा करें !
आपका अपना ही,
स्वामी शिवानन्द
निद्रा की कहानी
निद्रा प्रकृति का श्रेष्ठ शक्तिवर्धक है। यह नाड़ियों और मस्तिष्क को शान्त तथा पुनर्नवीन करती है। गहन निद्रा में ऊर्जा और शक्ति के सतत प्रवाहक स्रोत आत्मा से मन का निकट सम्पर्क होता है। इस कारण आप गहन निद्रा के बाद विश्रान्त और शान्त अनुभव करते हैं। नींद का उद्देश्य शरीर और मन के कार्यों में व्यय हुई ऊर्जा का पुनः संग्रहण करना है।
शरीर में होने वाले आधारभूत परिवर्तन जो नींद का कारण होते हैं, वे अभी तक समझे नहीं जा सके हैं। नींद का शारीरिक कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में अवश्य बहुत-कुछ जाना जा सकता
नींद स्तरों में आती है। विचार धीरे-धीरे रुक जाते हैं। आपके चारों ओर के वातावरण के प्रति सजगता धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। मन स्वयं को पुराने घटनाक्रम में उलझा लेता है। पुराने अनुभवों की यादें भीतर आ जाती हैं। यह स्वप्नावस्था है । तब आप पूर्ण रूप से अचेत हो जाते हैं। तब विचारों का पूरी तरह अन्त हो जाता है। प्रारम्भ में कुछ अचानक झटका लगने-जैसी गतिविधियाँ रहती हैं। श्रवण, दृष्टि तथा स्पर्श की संवेदना अत्यन्त कठिनाई से अनुभव हो पाती है। बाद में मांसपेशियाँ पूर्ण विश्राम की स्थिति में आ जाती हैं।
जब आप सोने जाते हैं, सबसे पहले दृष्टि-संवेदना जाती है, उसके वि बाद स्पर्श की संवेदना और अन्त में सुनने की संवेदना जाती है। जब आप निद्रा से जागते हैं, सबसे पहले सुनने की संवेदना कार्य करती है, उसके बाद स्पर्श की संवेदना, उसके बाद दृष्टि की संवेदना कार्य करती है।
इन तीनों में से दृष्टि या नेत्रेन्द्रिय में ही एक द्वार हैं पलकें, जो स्वयं बन्द हो सकती हैं। इसलिए यह सबसे पहले जाती है। अन्य दोनों में से श्रवणेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय से अधिक सूक्ष्म है। इसलिए श्रवणेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय से पहले काम करना बन्द करती है। यही कारण है कि कड़े बिस्तर पर आवाजें आपको जगाये रखती हैं। इसी तरह जब आप जागते हैं, तो श्रवणेन्द्रिय पहले कार्य आरम्भ करती है, उसके बाद आपको अनुभव होता है (क्योंकि तब स्पर्शेन्द्रिय कार्य आरम्भ करती है), उसके बाद आप अपनी आँखें खोलते हैं और दृष्टि-इन्द्रिय अपना खेल प्रारम्भ करती है।
अंग और मांसपेशियाँ कार्य करती हैं। राग-द्वेष वृत्तियाँ कार्य करती हैं। आपके शरीर के महत्त्वपूर्ण अंग उनकी क्षति-पूर्ति से अधिक काम करते हैं। इसका परिणाम होता है थकान । थकान के कारण मांसपेशियाँ विश्राम चाहती हैं और नींद प्रकट होती है।
भरा हुआ पेट, आमाशय या मूत्राशय, श्वसन में कष्ट, असुविधाजनक बिस्तर, चुस्त या तंग कपड़े, आवाजें, तीव्र प्रकाश, इच्छाएँ, काफी, चाय, विटामिन बी की कमी, चिन्ता, भय, व्याकुलता, सोने का अनियमित समय, सिनेमा, रात के समय उत्तेजक उपन्यास पढ़ना, दुःख, असफलता, निराशा—ये सभी निद्रा में बाधक हैं।
एक अँधरे शान्त कमरे में सोयें। घड़ी को बन्द कर दें । प्रशामक या निद्राजनक औषधि न लें। शिथिलीकरण क्रिया सीखें। रात के समय उत्तेजना, उत्तेजक पदार्थों तथा तीव्र मानसिक कार्यों न करें। शीघ्र सोने चले जायें। मन्द गति से आती गहरी नींद में लीन हो जायें। आप अच्छी, विश्रान्तिदायक, गहन निद्रा का आनन्द उठायेंगे।
अन्तिम शब्द
ईश्वर के सामने सम्पूर्ण, निःसंकोच और बिना किसी शर्त के आत्म-समर्पण करें।
यह शान्तिपूर्ण, अति-विश्रान्तिदायक और वास्तविक गहन निद्रा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है।
यह आत्मसाक्षात्कार-प्राप्ति हेतु, जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्ति हेतु और स्थायी शान्ति, अवर्णनीय सुख और अमरत्व के उपभोग हेतु एकमात्र मार्ग है।
निद्रा का कोई स्थानापन्न नहीं है। संसार की समस्त औषधियाँ भी आपकी सहायता नहीं कर सकतीं।
आत्मसाक्षात्कार का कोई स्थानापन्न नहीं है। तीनों लोकों की सम्पत्ति भी आपकी सहायता नहीं कर सकती।
जब कोई सो जाता है, नहीं जानता । उसके भीतर क्या होता है, यह कोई भी नहीं जानता ।
जब तीनों अवस्थाएँ पार हो जाती हैं, पाँचों कोष पार हो जाते हैं और अज्ञान दूर हो जाता है तथा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब ठीक-ठीक क्या होता है, यह कोई नहीं जानता ।
जितना आप गहरी निद्रा लाने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही अधिक नींद आपसे दूर भागेगी।
जितना अधिक आप स्वार्थ-भावना, कर्तृत्व-भोक्तृत्व अभिमान, राग-द्वेष, वासनाओं और तृष्णाओं तथा अन्य दुर्गुणों को अपने अन्तर्मन में रख कर कार्य करेंगे, आत्मसाक्षात्कार आपसे उतना ही दूर चला जायेगा।
आपके भीतर स्थित आत्मा की कृपा के बिना नींद आना सम्भव नहीं है।
आत्मसाक्षात्कार भी आपके भीतर स्थित आत्मा (या ईश्वर) की कृपा के बिना सम्भव नहीं है।
इसलिए प्रार्थना करें, उनके नाम गायें, उनका ध्यान करें और उनके सामने निःसंकोच बिना किसी शर्त के पूर्ण आत्म-समर्पण करें।
अनिद्रा हेतु उनसे प्रार्थना कीजिए— “मैं आपका हूँ, सब आपका है; मेरे ईश्वर, आप ही सब करेंगे।” यह अचूक औषधि है।
और, यह अविद्या से उत्पन्न दुःखों के लिए अचूक औषधि है। यह परमानन्द, स्थायी शान्ति और अमरत्व के प्रदेश के प्रवेश-द्वार की कुंजी है।
इस अमृत का पान कीजिए तथा गहन निद्रा और समाधि का आनन्दोपभोग कीजिए ।
परिशिष्ट
प्रेरक सन्देश और गीत
आजकल जीवन बहुत जटिल हो गया है। अस्तित्व के लिए भयंकर संघर्ष है। मनुष्य को बड़ी-बड़ी दर्शनशास्त्र की पुस्तकों तथा धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ने का समय नहीं है। नीचे कुछ संक्षिप्त योग की गोलियाँ या दार्शनिक या आध्यात्मिक गोलियाँ सन्देशों या भक्ति-गीतों के रूप में सोने के लिए जाने के पूर्व सरल अभिशोषण तथा सरल अवशोषण हेतु दी गयी है। आप परम शान्ति या परमानन्द का उपभोग करेंगे। यह स्वाध्याय या धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन और ध्यान का एक प्रकार होगा। आप धीरे-धीरे दिव्य जीवन हेतु प्रेरित होंगे। आप दुःस्वप्नों से मुक्त होंगे। आपका मन सत्त्व से आपूरित हो जायेगा। आपको विश्रान्तिदायक नींद आयेगी। आप धीरे-धीरे मन के सन्तुलन, आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति और दृढ़ संकल्प शक्ति का विकास करेंगे। आपके भीतर आध्यात्मिक जीवन हेतु इच्छा जाग्रत हो जायेगी। यह आपके लिए ध्वनियों, कलह और कोलाहल से भरे संसार में भी निरन्तर सत्संग होगा। आपको योगियों की खोज में इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सा धन बचा पायेंगे। इन शिक्षाओं की शक्ति के साथ जियें और मोक्ष या मुक्ति इसी जन्म में प्राप्त करें।
दिव्य जीवन जियें
मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। ईश्वर वह पदार्थ है जिससे वह बना है। हम उसके प्रकाश में जीते और विचरण करते हैं। सभी में परम आध्यात्मिक चेतना छिपी हुई है। यह ईश्वर का सिद्धान्त है जो एक ओस की बूँद के चारों ओर है, यह उसका जीवन है जो छोटे-से-छोटे पौधे में. छोटे-से-छोटे प्राणी में, छोटी-से-छोटी कोशिका में स्पन्दित हो रहा है। यह उसकी ही शक्ति है जो एक कली को खिलने योग्य बनाती है। ईश्वर के की कमी ही जीवन के समस्त दुःखों और अव्यस्थाओं तथा ससार के का मूल है। सच्चा सुख और समस्त जीवन का वास्तविक आनन्द ईश्वर के ज्ञान में तथा अपनी दिन-प्रति-दिन की गतिविधियों को उनके प्रकाश में तथा उनके मार्गदर्शन में सम्पादित करने में सन्निहित है।
जीवन का स्वस्थ दर्शन ही समस्त मानव-जाति के समस्त पापों की रामबाण औषधि है। भय और व्याकुलता की मनोदशा जो कि मनुष्य और जगत् को दुःखी करती है, उसके लिए अचूक औषधि उस ईश्वर में आस्था है जिसके एक अणु ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को व्याप्त किया है और धारण किया। हुआ है। इसलिए ज्ञान के लिए, जीवन के धार्मिक दर्शन के लिए तथा ज्ञानवर्धन हेतु प्रयत्न करें। ईश्वर के प्रति आस्था रखें और उसे उग्र करें। अभ्यास करना आपके लिए श्रेष्ठ है। आपके भीतर जो अनावश्यक है, उसे निकाल फेंकें और ईश्वर का दर्शन करें। विकसित हों। दिव्य जीवन के सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतारें। अब आप अपनी आँखों पर तुच्छ वासनाओं और महत्त्वाकांक्षाओं का परदा न पड़ने दें। अपने अन्तर में स्थित तेज तथा ईश्वर के सच्चे संसार को जो इस जगत् से परे है, को छुपने न दें। दिन-प्रति-दिन आप बुद्धिमान्, योग्य और दिव्य बनते जायेंगे ।
शुद्धता और पवित्रता का वैभवशाली तथा निष्कलंक जीवन जियें और आप सिद्ध करें कि आप ईश्वर के प्रतिरूप हैं जैसे कि प्रत्येक सन्त और ऋषियों ने सिद्ध किया। प्रत्येक सन्त, ऋषि और तत्त्वज्ञानी का जीवन हमें इस जीवन और इस जगत् की नश्वरता और ईश्वर की सत्यता को, हमारे आन्तरिक शासक को और परलोक को हमें दिखाता है। उन महान् आत्माओं के पदचिह्नों पर चलने हेतु विशेष प्रयत्न कीजिए और सन्त,
ऋषि, तत्त्वज्ञानी, आध्यात्मिक नायक, सिद्धि, शक्ति, शान्ति तथा आनन्द मैं विकास कीजिए।
थोड़े से सच्चे आध्यात्मिक अभ्यास, प्रेमपूर्ण हृदय, सेवा करने वाले हाथ, कुछ मिनटों की प्रार्थना, कुछ समय तक उनके दिव्य गुणों का ध्यान, स्वच्छ मन, दृढ सकल्प-शक्ति, धैर्य और अध्यवसाय —ये ही स्थायी शान्ति और परमानन्द हेतु मार्ग या श्रेष्ठ विधियाँ हैं।
आपकी यथार्थ प्रकृति
प्रिय अमर आत्मन्!
ईश्वर को जानने और पूजन की आस्था का ही नाम धर्म है। यह किसी क्लब की मेज पर बहस का विषय नहीं है। यह यथार्थ आत्मज्ञान या साक्षात्कार है। यह मानव के अन्तर्मन की अभिलाषा की पूर्ति है । इसलिए जीवन के परम लक्ष्य की तरह धर्म का पालन कीजिए। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण इसके साक्षात्कार के लिए जियें । बिना धर्म के जीवन वास्तविक मृत्यु है।
अपने विचारों का विश्लेषण करें। अपने उद्देश्यों का अनुरीक्षण करें। स्वार्थपरता छोड़ें। लालसाओं को शान्त करें। इन्द्रियों को नियन्त्रित करें। अहंकार को नष्ट करें। सबकी सेवा करें। सबसे प्रेम करें। अपने हृदय को शुद्ध करें। मन के मैल को साफ करें। सुनें और विचार करें। एकाग्रता और ध्यान करें। आत्मसाक्षात्कार करें।
कुछ है जो सम्पत्ति से अधिक मूल्यवान् है। कुछ है जो आपकी पत्नी से अधिक मूल्यवान् है। कुछ है जो आपके बच्चों से अधिक मूल्यवान् है। और कुछ आपके स्वयं के जीवन से भी अधिक मूल्यवान् है। यह मूल्यवान् वस्तु आपकी आत्मा, अन्तर्यामी, अमरत्व है। इस अमर आत्मा का साक्षात्कार मात्र ध्यान के अनवरत अभ्यास द्वारा ही हो सकता है। है सौम्य । प्रिय अमर आत्मा। साहसी बनो! आनन्दित रहो।
हे सौम्य! प्रिय अमर आत्मा ! साहसी बनो आनन्दित रहो ।चाहे आप बेरोजगार है, चाहे आपके पास खाने को कुछ न हो, चाहे आप चिथड़ों में लिपटे हों, आपकी यथार्थ प्रकृति सच्चिदानन्द है। आपका बाह्य आवरण यह नाशवान् भौतिक शरीर माया का मिथ्या मोह-जाल है। मुस्करायें, सीटी बजायें, हँसें, कूदें, खुशी से नाचें। 'ॐ ॐ ॐ', 'राम राम राम गायें। इस मांस के पिंजरे से बाहर आये। आप यह नाशवान् शरीर नहीं हैं। आप अलिंग आत्मा है। आप वह आत्मा हैं जो आपकी हृदय गुहा में निवास करती है। उसी भाँति व्यवहार करें। ऐसा ही अनुभव करें। कल या परसों से नहीं, इसी क्षण से अपने जन्म सिद्ध अधिकार को माँगे । 'तत्त्वमसि।' आप वह है, अनुभव करें, स्वीकार करें, साक्षात्कार करें, पहचानें, मेरे प्रिय राम!
अपने केन्द्र का पता लगायें। सदा अपने केन्द्र में निवास करें। यह केन्द्र ही परमानन्द और आन्तरिक सूर्य के प्रकाश का धाम है। यह केन्द्र ही परमधाम, परमगति या परमलक्ष्य है। यह केन्द्र ही आपका मौलिक, सुन्दर वास-स्थान, अमरत्व और निर्भयता का धाम है। यह केन्द्र आत्मा या ब्रह्म है। यह अविनाशी ब्रह्म-स्थान, अप्रतिम वैभव तथा कीर्ति का स्थान है।
भक्तियोग
हरि ॐ ! हरि ॐ ! हरि ॐ !
ज्योतिपुत्र !
भक्ति ईश्वर के समक्ष प्रबल भावना युक्त समर्पण है। भक्ति समस्त धार्मिक जीवन का आधार है। भक्ति वासनाओं और अहंकार का नाश करती है । भक्ति मन को महान् ऊँचाई तक ले कर जाती है। भक्ति ज्ञान के प्रकोष्ठ की कुंजी है। भक्ति का अन्त ज्ञान में होता है। भक्ति दो से प्रारम्भ हो कर एक में समाप्त होती है। पराभक्ति और ज्ञान एक है।
प्रेम से ऊँचा कोई सद्गुण नहीं, प्रेम से बढ़ कर कोई कोषागार नहीं. प्रेम से ऊँचा कोई धर्म नहीं; क्योंकि प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम और भक्ति समानार्थी शब्द है। यह संसार प्रेम से ही प्रकट हुआ है, इस जगत् का प्रेम में अस्तित्व है और यह प्रेम में ही समाप्त हो जायेगा। ईश्वर प्रेम की मूर्ति है। उसकी प्रकृति के प्रत्येक कण-कण में आप उसके प्रेम को वास्तव में समझ सकते हैं। I
प्रेम, विश्वास और भक्ति से रहित जीवन नीरस और व्यर्थ है। यह सच में मृत्यु है। प्रेम दिव्य है। प्रेम इस पृथ्वी पर सबसे महान् शक्ति है। यह अटल है। एकमात्र प्रेम ही किसी मनुष्य के हृदय को जीत सकता हैं। प्रेम शत्रु का वशीभूत कर सकता है। प्रेम जंगली और मांसाहारी जानवरों को भी पालतू बना सकता है। इसकी गहराई असीम है। इसकी प्रकृति अवर्णनीय है। इसकी महिमा अवर्णनीय है । प्रेम धर्म का सार है। इसलिए शुद्ध प्रेम का विकास करो ।
अपनी हृदय-गुहा में प्रेम की ज्योति जलाओ। सबसे प्रेम करो। अपने प्रेम के आलिंगन में सभी प्राणियों को सम्मिलित करें। विश्व-प्रेम की भावना, सभी को स्वीकार करने का भाव और दिव्य प्रेम का विकास करें। प्रेम एक रहस्यमय सरेस है जो सभी के दिलों को जोड़ता है। यह उच्च शक्तिशाली दिव्य चमत्कारिक आरोग्यकर लेप है। अपने सभी कार्यों को शुद्ध प्रेम से आप्लावित करें। चालाकी, लालच, धूर्तता और स्वार्थ-परायणता को नष्ट करें। दयालुता के कार्य सदा करते रहने पर ही अमरत्व प्राप्त होता है। प्रेमपूर्ण हृदय के साथ सदा सेवा कार्य करने पर ही द्वेष, घृणा, क्रोध और ईर्ष्या दूर किये जा सकते हैं। करुणा, दान और सेवा के अभ्यास से हृदय शुद्ध तथा कोमल होता है और ये हृदय-कमल का विकास करते हैं तथा आकांक्षी को दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने हेतु तैयार करते हैं।
प्रेम में जियें। प्रेम में साँस लें। प्रेम में गायें। प्रेम खायें। प्रेम पियें। प्रेम से विचार करें। प्रेम में चलें। प्रेम से बोलें। प्रेम से प्रार्थना करें। प्रेम में 1 ध्यान करें। प्रेम में विचरण करें। प्रेम में लिखें। प्रेम में मरें। दिव्य प्रेम के अमृत का पान करें और प्रेम-मूर्ति (प्रेम-विग्रह ) बन जायें।
आत्म-साक्षात्कार
ज्योतिपुत्रो !
इस जगत् के खेल के पीछे, इन भौतिक घटनाओं के पीछे, इन नाम-रूपों के पीछे भावनाओं, विचारों, आवेगों तथा कल्पनाओं के पीछे, मूक साक्षी, आपके अमर मित्र और शुभ-चिन्तक, वह पुरुष या जगद्गुरु, अन्तर्यामी, अज्ञात योगी, चेतना की अदृश्य शक्ति या गुप्त ऋषिनिवास करते हैं। वह ही एकमात्र स्थायी सत्य या जीवित सत्य हैं। वह ही ब्रह्म, परमात्मा या अनन्त हैं। वह आत्मा हैं। इस परिवर्तनशील दृश्यमान् जगत् के पीछे जो सत्यता है, उसका साक्षात्कार करना ही मानव-जीवन का लक्ष्य है। मानव मात्र का परम लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करना है। आत्म-साक्षात्कार मात्र ही आपको पूर्ण स्वतन्त्र या मुक्त बना सकता है। अपने शरीर, मन और इन्द्रियों पर विश्वास न कीजिए। आन्तरिक आध्यात्मिक जीवन बितायें। स्थिर भक्ति और संयम द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करें। अमरत्व का मधु पियें और संसार की ज्वालाओं का दमन करें और इसकी यन्त्रणाओं, कष्टों तथा दुःखों को कम करें।
मित्रो! क्या भोजन, शयन और बात करना-इनके सिवा जीवन का कोई उच्च लक्ष्य नहीं है? क्या इन क्षणिक और मायावी सुखों से अधिक श्रेष्ठ आन्तरिक आनन्द का कोई रूप नहीं है?
क्या भौतिक जीवन में अनिश्चित है? इस भूलोक पर जीवन, हमारा अस्तित्व कितना अजी कपद है? क्या अब हमे ऐसे स्थान पर दिव्य वैभव के परम धाम आन्तरिक सूर्यका पूर्ण शान्ति है और है प्रयत्न नहीं करना चाहिए।
आओ, आओ, योगी बन अपने आओ सभी कुसंस्कारों को नष्ट कर दो ऊँचा रख एडवोकेट या चिकित्सक वा इंजीनियर या व्याख्याता बनना आपकी सबसे उच्च महत्त्वाकांक्षा होगी। किन्तु क्या यह आपको मुक्ति देगी? क्या ह आपको परमानन्द देगी? क्या यह आपको स्थायी शान्ति देगी? क्या यह आपको अमर बनायेगी? क्या आप सिद्धि या अमरत्व प्राप्त नहीं करना चाहते? क्या आप जीवन के परम लक्ष्य- कैवल्य या मुक्ति आत्म-स्वराज्य को प्राप्त करना नहीं चाहते? तो आइए, उच्च वस्तुओं के लिए प्रयत्न करें। साहसी बनें। पीछे न देखें, आगे बढ़ें। पता लगायें, मैं कौन हूँ? ध्यान दें, विचार करें, ध्यान करें और आत्मिक वैभव का साक्षात्कार करें।
ॐ सत्-चित्-आनन्द है, ॐ अनन्त है, ॐ नित्यता है, ॐ- अमरता है। ॐ गाओ! ॐ का नाद करो! ॐ का अनुभव करो!
दिव्य जीवन
हरि ॐ ! हरि ॐ ! हरि ॐ !
दिव्य जीवन ईश्वर में या अमर आत्मा में जीवन है। जो दिव्य जीवन व्यतीत करता है, वह देखभाल, चिन्ताओं, आकुलताओं, कष्टों, दुःखों और क्लेशों से मुक्त रहता है। वह अमरता, सिद्धि, मुक्ति, स्वतन्त्रता, अनन्त शान्ति, परमानन्द और चिरस्थायी सुख का उपभोग करता है। वह सभी जगह प्रसन्नता, शान्ति और प्रकाश फैलाता है।
दिव्य जीवन व्यतीत करने के लिए आपको वन में निवास करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस संसार में रहते हुए भी दिव्य जीवन जी सकते। है। जो चाहिए, वह है स्वार्थपरायणता, मेरे पन की भावना, अनुराग, वासनाओं और तृष्णाओं का संन्यास। अपने मन को ईश्वर को और हाथों को मानवता की सेवा हेतु समर्पित कर दीजिए।
मानवता की सेवा आत्म-भाव से कीजिए। निर्धनों की सेवा कीजिए। बीमारों की सेवा नारायण-भाव से कीजिए। समाज की सेवा कीजिए। देश की सेवा कीजिए। निष्काम सेवा सबसे उच्च योग है। जो सेवा में आत्मा से लगा है, उसका हृदय जब शुद्ध हो जायेगा, तो उसके लिए बिना किसी प्रयत्न के समाधि स्वयं ही आयेगी। सेवा ईश्वर की पूजा है, इसे कभी न भूलें। वह जो चम्मच में ब्रह्म या अमर आत्मा को देखता है, औषधि और रोगी में ब्रह्म का दर्शन करता है, चिकित्सक में ब्रह्म को देखता है, सेवा में ब्रह्म को देखता है—जो सेवा करते समय ऐसा सोचता या ऐसा ध्यान करता है, वास्तव में वह ब्रह्म या ईश्वर तक पहुँचता है।
ब्रह्मचर्य का पालन आध्यात्मिक प्रगति हेतु बहुत आवश्यक अमरत्व-प्राप्ति का आधार ब्रह्मचर्य है। यह स्वयं दिव्य जीवन है। ब्रह्मचर्य भौतिक प्रगति तथा आध्यात्मिक उन्नति लाता है। यह आत्मा में शान्तिपूर्ण जीवन का आधार है। यह आन्तरिक राजसिक बलों— काम, क्रोध, लोभ आदि को नियन्त्रित करने के लिए शक्तिशाली अस्त्र है। यह असाधारण ऊर्जा, विशाल संकल्प-शक्ति और अच्छी विचार-शक्ति प्रदान करता है।
योग या दिव्य जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग जप है। मन्त्र दिव्यता है। मन्त्र को बार-बार दोहराने या ईश्वर के नाम को बार-बार दोहराने को जप कहते हैं। कलियुग में मात्र जप का अभ्यास ही अनन्त शान्ति, सुख और अमरत्व को दे सकता है। जप का अन्तिम परिणाम समाधि या ईश्वर के साथ साक्षात्कार होता है।
भगवान् के नाम को विश्वास और भक्ति के साथ गाना ही संकीर्तन कहलाता है। जब आप उनके नाम को गाते हैं, तो अनुभव करें कि भगवान् हरि या आपके इष्टदेवता आपके हृदय में बैठे हैं, यह कि भगवान् का प्रत्येक नाम दिव्य शक्ति से पूर्ण है। यह कि पुराने कुसंस्कार और वासनाएँ नाम की शक्ति से जल गयी हैं और मन सत्त्व तथा पवित्रता से आपूरित हो गया है। यह कि रजोगुण और तमोगुण पूर्णतया नष्ट हो गये हैं और अज्ञानता का आवरण फट गया है। इस प्रकार के मनोभाव से सकीर्तन के सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगे। जप की संख्या या कीर्तन के समय को आध्यात्मिक प्रगति नहीं समझना चाहिए, बल्कि भगवान् का नाम जिस तीव्र भाव से गाया जाता है, उसे आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं।
याज्ञवल्क्य - मैत्रेयी संवाद
बृहदारण्यक उपनिषद्
ॐ ॐ !ॐ !
याज्ञवल्क्य ऋषि जो एक महान् मनीषि थे, वे बोले, “मैत्रेयी! वास्तव में अब मैं इस घर को त्याग कर अगले वर्णाश्रम-जीवन (संन्यास) हेतु वन में जा रहा हूँ । इसलिए मैं अपनी सम्पत्ति को तुम्हारे और कात्यायनी के मध्य बाँटना चाहता हूँ।”
मैत्रेयी बोली, "मेरे पूज्य स्वामी, यदि सारा संसार और उसकी सारी सम्पत्ति मेरे पास हो, तो बताइए कि क्या मैं सच में अमरत्व को प्राप्त कर सकूँगी ?”
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, "नहीं, तुम्हारा जीवन धनिक जनों की तरह होगा; किन्तु सम्पत्ति के द्वारा अमरता प्राप्त करने की कोई आशा नहीं है।"
" सम्पत्ति मेरे लिए किस काम की होगी, यदि मैं इससे अमर न हो सकूँ। मेरे पूज्य स्वामी, जो आपको ज्ञात हो, ऐसे अपरत्व प्राप्ति के साधन मुझे बतलाइए।
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, "प्रिय मैत्रेयी, आओ, मैं तुम्हें बताता है। कह रहा हूँ, उसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करो।"
याज्ञवल्क्य बोले, "वास्तव में पति के हितार्थ पति प्रिय नहीं होता, प्रत्युत् आत्मा के हितार्थ पति प्रिय होता है। वास्तव में पत्नी के लाभार्थ पत्नी प्रिय नहीं होती, प्रत्युत् आत्मा के लाभार्थ पत्नी प्रिय होती है। वास्तव में पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, प्रत्युत् आत्मा के लिए पुत्र प्रिय होता है। वास्तव में यह अमर सर्वव्यापक (आत्मा या ब्रह्म) को ही सदा देखा, सोचा, ध्यान दिया और ध्यान किया जाता है। हे मैत्रेयी, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।
"है मैत्रेयी, जब द्वैतभाव होता है, तो एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को सूंघता है, एक दूसरे का स्वाद लेता है, एक दूसरे को प्रणाम करता है। एक दूसरे से बात करता है। एक दूसरे को सुनता है। एक दूसरे को स्पर्श करता है, एक दूसरे को जानता है। किन्तु जब सबमें एक ही आत्मा है, यह भाव होगा तो कैसे एक दूसरे को देख सकेगा, कैसे वह दूसरे को सूँघ सकेगा, स्पर्श करेगा, जानेगा? वह उसे कैसे जानेगा जिसके द्वारा वह सबको जानता है? इसी आत्मा को 'नेति नेति' (नहीं-नहीं) करके वर्णित किया गया है। आत्मा या परमात्मा अविनाशी है। वह मुक्त और निरासक्त है। उसको दर्द नहीं होता, न ही उसका नाश होता है। कोई भी जानने वाले को कैसे जान सकता है ? इस प्रकार हे मैत्रेयी, मैंने तुम्हें निर्देश दिया (ज्ञान दिया)।"
इतना कह कर याज्ञवल्क्य वन को चले गये ।
मुक्ति का सन्देश
ॐ !
अमरता के पुत्रो !
"ईश्वर आपके भीतर है। वह सभी प्राणियों के हृदय में बैठे हैं। जो कुछ भी आप देखते हैं, सुनते, स्पर्श या अनुभव करते हैं, वह ईश्वर है। इसलिए किसी से घृणा न करो, किसी को मत छलो, किसी को चोट न पहुँचाओ। प्रेम करो और सबके साथ एक हो जाओ। आप शीघ्र ही परमानन्द को प्राप्त करेंगे। आत्म-संयमी बनें। विचारों, भावनाओं, आहार और वस्त्र में सरलता और समन्वय करें। सबसे प्रेम करें। किसी से भयभीत न हों। जड़ता, आलस्य और भय को दूर करें। सत्यान्वेषी बनें। धर्म के नियम को समझें। सदा जागरूक और चौकन्ने बनें। दुःख और प्रतिकूलता को जिज्ञासा और विचार के द्वारा जीतें। प्रतिक्षण मुक्ति, सिद्धि और परमानन्द की ओर बढ़ें। क्या आप सबके मध्य ऐसा कोई व्यक्ति है जो जोर से और बलपूर्वक कह सके, “अब मैं योग्य साधक हूँ। मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। मैंने स्वयं को चतुस्साधनों से सज्जित किया है। मैंने अपने हृदय को निष्काम सेवा, कीर्तन और जप द्वारा शुद्ध किया है। मैंने गुरु की आस्था और समर्पण से सेवा की है तथा उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त किया है?” ऐसा मनुष्य संसार की रक्षा कर सकता है। वह शीघ्र ही एक दिव्य मशाल, एक अद्वितीय ज्ञान की मशाल धारण करने वाला, एक दिव्य योगी बन जायेगा। हे मानव, स्वयं को अब तैयार रखो। यह बड़ी ही शर्मनाक बात है कि तुम अभी तक अज्ञानी हो और अपना जीवन आहार, पीने, सोने, बेकार की गपशप और निरर्थक कामों में व्यर्थ गँवा रहे हो। अभी तक तुमने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। घड़ी निकट आ रही है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इसी क्षण से भगवान् के नाम का स्मरण प्रारम्भ कर दो ईमानदार और उत्साही बनें। सबसे प्रेम करें। आप स्वयं को उनकी कृपा योग्य बना लेंगे। आप जन्म और मृत्य के भीषण सागर को पार कर सकेंगे और परमानन्द तथा अमरत्व को प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान में एक दिन के लिए भी न चूकें। नियमितता सबसे अधिक आवश्यक है। जब मन थका हो, इसे एकाग्र न करें। इसे थोड़ा विश्राम दें। रात के समय भारी भोजन न लें। यह आपके प्रातः कालीन ध्यान में विघ्न डालेगा। जप, कीर्तन, प्राणायाम, सन्तों का सत्संग, शम, दम और यम का अभ्यास, सात्त्विक या शुद्ध भोजन, धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय, ध्यान, विचार—ये सभी मन को नियन्त्रित करने और परमानन्द-प्राप्ति तथा अमरत्व की प्राप्ति में सहायक होंगे। यदि आपके मन में बुरे विचार आयें, तो आप उन्हें बलपूर्वक दूर करने का प्रयत्न न करें, इससे आप अपनी शक्ति क्षीण करेंगे । ॐ !
विद्यार्थियों को सलाह
ॐ! मित्रो !
आप मातृभूमि के भविष्य की आशा हैं। आप कल के नागरिक हैं। आपको सदा जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचना तथा लक्ष्य-प्राप्ति हेतु जीवन जीना चाहिए। जीवन का लक्ष्य सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति या कैवल्य या जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। पूर्ण नियमित सदाचारी जीवन व्यतीत करें। नैतिक बल आध्यात्मिक प्रगति की रीढ़ है। नैतिक संस्कृति आध्यात्मिक साधना का भाग है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्राचीन समय में ऋषियों ने ब्रह्मचर्य-पालन से अमरता प्राप्त की। ब्रह्मचर्य नवीन शक्ति, ओज, जीवनी-शक्ति, जीवन में सफलता और परमानन्द का स्रोत है। वीर्य-शक्ति का ह्रास रोगों, कष्टों और पूर्वकालिक मृत्यु का कारण है। इसलिए इस वीर्य ऊर्जा के संरक्षण हेतु विशेष सावधान रहें । ब्रह्मचर्य के अभ्यास से अच्छा स्वास्थ्य, आन्तरिक शक्ति, मन की शान्ति और दीर्घायु प्राप्त होती है। यह मन तथा नाड़ियों को शक्ति प्रदान करता है और शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा के संरक्षण में सहायक होता है। यह साहस और शक्ति में वृद्धि सामना है तथा करता । यह दैनिक जीवन-संग्राम में आने वाली कठिनाइयों का करने की शक्ति देता है। एक पूर्ण ब्रह्मचारी संसार को चला सकता प्रकृति और पंचतत्त्वों पर ज्ञानदेव की तरह शासन कर सकता है। वेदों में और मन्त्रों की शक्ति में आस्था विकसित कीजिए। नित्य ध्यान का अभ्यास कीजिए। सात्त्विक भोजन लीजिए। पेट को अधिक न भरें। अपनी गलतियाँ सुधारें। अपने दोषों को स्वीकार करें। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठे बहाने न गढ़ें। झूठ न बोलें। प्रकृति के नियमों का अनुसरण करें। नित्य भरपूर व्यायाम करें। अपने कर्तव्यों को समय पर पूरा करें। सादा जीवन उच्च विचार का विकास करें। अन्धानुकरण त्याग दें। आपने बुरी संगति के कारण जो कुसंस्कार सीख लिये हैं, उनको बदलें। गीता, उपनिषद्, योगवासिष्ठ, ब्रह्मसूत्र तथा श्री शंकराचार्य जी के ग्रन्थों और अन्य धर्मग्रन्थों का स्वाध्याय करें। उनमें ही आप वास्तविक सुख और शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। कुछ पश्चिमी तत्त्वज्ञानी कहते हैं—“हम जन्म और धर्म से हिन्दू नहीं हैं; किन्तु मन जिस शान्ति को चाहता है और आत्मा जिस सन्तोष को चाहती है, वह हम पूर्व के ऋषियों के उपनिषदों में ही प्राप्त करते हैं।” हमें सबके साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। सबसे प्रेम करें। सबकी सेवा करें।
अनुकूलता का विकास करें और निष्काम सेवा के प्रति उत्साह रखें तथा अथक सेवा द्वारा सभी के हृदयों में प्रवेश करें। यही वास्तव में एकत्व का अद्वैतिक साक्षात्कार है । ॐ!
हृदय को झंकृत करने वाले कीर्तन
कीर्तन की क्रियाविधि: सभी लोग एकत्र हैं, उन्हें इन ध्वनियों को एक-साथ मिल कर एक धुन में गाना चाहिए। कहीं भी विराम नहीं होना चाहिए। जब एक व्यक्ति श्वास लेने के लिए रुके, उस समय दूसरा इसे चालू रखे और कीर्तन की समाप्ति होने तक कोई अन्तराल नहीं होना चाहिए। मन को कीर्तन के स्पन्दनों से पूर्ण हो जाना चाहिए। आपको ऐसा अनुभव करना चाहिए कि मन्त्र आपको अन्तर तक प्रभावित कर रहा है. आपके भीतर चारों ओर से प्रविष्ट हो रहा है। ये ध्वनियाँ भाव-समाधि के लिए सरल विधि है। इनको सोने से पहले थोड़ी देर तक गायें। ये मन को शान्त करेंगी, इसे सत्त्व से परिपूर्ण कर देंगी और निश्चित ही गहरी नींद प्रदान करेंगी।
१. जय जय राधे गोविन्द ।
२. सीता राम राम राम ।
३. राम राम राम राम राम ।
४. विट्ठला विठ्ठला, जय जय विठ्ठला ।
५. रामकृष्णा गोविन्दा, जय जय गोविन्दा ।
६. जय मन मोहना, राधा मन मोहना
७. आजा रे मोहन, आजा रे मोहन.... अब आजा रे मोहन, आजा रे ।
८. हरे कृष्ण हरे राम, राधे कृष्ण राधे श्याम ।
९. गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण |
१०. कृष्ण मुरारी गिरिवर धारी।
नीचे दी गयी ध्वनियाँ अलग प्रकार के हृदय को झंकृत करने वाले कीर्तन हैं। इन ध्वनियों की प्रथम पंक्ति पहले की तरह एक भक्त द्वारा गायी जाती हैं तथा अन्य उसे दोहराते हैं। अन्तिम पंक्तियाँ जो मोटे अक्षरों में हैं, उन्हें सभी साथ-साथ हैं ऊपर ही की भाँति । ये कीर्तन-ध्वनियाँ भक्तों के मन को सामूहिक रूप से प्रभावित करती हैं (समष्टि कीर्तन) ।
११. गोविन्दा गोविन्दा गोपाल रामा |
गोपाला गोपाला गोविन्द रामा ।
गोविन्दा रामा, गोपाला रामा ।
गोविन्दा, गोविन्दा, गोविन्दा, गोविन्दा ।।
१२. (अष्टाक्षर कीर्तन)
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
बदरी नारायण नारायण नारायण
हरि ॐ नारायण नारायण नारायण
सूर्य नारायण नारायण नारायण
हरि ॐ, हरि ॐ, हरि ॐ, हरि ॐ
(लम्बा खींच कर गायें)
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल
(लम्बा खींच कर गायें)
नारायण नारायण नारायण नारायण
महामन्त्र कीर्तन
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे;
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
राम धुन लागी
राम धुन लागी,
गोपाल धुन लागी,
कैसे छुटे ये राम धुन लागी ।
गोविन्द जय जय
गोविन्द जय जय गोपाल जय जय
राधारमण हरि गोविन्द जय जय
शंकर जय जय शम्भो जय जय
उमा रमण शिव शंकर जय जय ।
प्रेम का गीत
(धुन: सुनाजा)
पिला दे, पिला दे, पिला दे कृष्णा,
तू प्रेम-भरा प्याला पिला दे कृष्णा;
दिखा जा, दिखा जा, दिखा जा कृष्णा,
वो माधुरी सी मूर्ति दिखा जा कृष्णा ।
लगा जा, लगा जा, लगा जा कृष्णा,
मेरी नैया को पार लगा जा कृष्णा ;
खिला दे, खिला दे, खिला दे कृष्णा,
माखन और मिश्री खिला दे कृष्णा ।
सुना जा, सुना जा, सुना जा कृष्णा,
वो बाँसुरी की तान सुना जा कृष्णा ।
सुना जा, सुना जा, सुना जा कृष्णा,
वो गीता वाला ज्ञान सुना जा कृष्णा ।
चिदानन्द का गीत
चिदानन्द चिदानन्द चिदानन्द हूँ,
हर हाल में अलमस्त सच्चिदानन्द हूँ।
अजरानन्द अमरानन्द अचलानन्द हूँ,
हर हाल में अलमस्त सच्चिदानन्द हूँ।
(अन्तराय)
निर्भय और निश्चिन्त चिद्घनानन्द हूँ,
कैवल्य केवल कूटस्थ आनन्द हूँ।
नित्य शुद्ध सिद्ध सच्चिदानन्द हूँ
(चिदानन्द चिदानन्द. .)
नालेज ब्लिस, नालेज ब्लिस,
ब्लिस एब्सोल्यूट इन ऑल कंडीशन,
आइ एम नालेज, ब्लिस एब्साल्यूट ।
आय एम विदाउट ओल्ड एज, बिदाउट डेथ, विडाउट मोशन,
इन आल कंडीशन आय एम नॉलेज,
ब्लिस एब्साल्यूट ।
(अन्तराय)
आय एम विदाउट फीयर
विदाउट वरी ब्लिस एब्साल्यूट
एक्जिस्टेंस एब्साल्यूट
नालेज एवसाल्यूट
इण्डिपेंडेंट, अनचेंजिंग नान- डुएल आत्मा
इमारटल आत्मा अद्वैत आत्मा
इटरनल प्योर, परफेक्ट नालेज, ब्लिस एब्साल्यूट
(चिदानन्द चिदानन्द. .)
शिवानन्द शिवानन्द शिवानन्द हूँ
अगड़ बम वाला बगड़ बम वाला अखिलानन्द हूँ।
चिदानन्द चिदानन्द चिदानन्द हूँ
हर हाल में अलमस्त सच्चिदानन्द हूँ।
निजानन्द निजानन्द निजानन्द हूँ
हर हाल में अलमस्त सच्चिदानन्द हूँ।
पाण्डुरंगाका गीत
जय जय विठ्ठला पाण्डुरंगा,
जय हरि विठ्ठला पाण्डुरंगा ;
जगन्निवास पाण्डुरंगा,
जगत्पति पाण्डुरंगा ;
सर्वान्तर्यामी पाण्डुरंगा,
सर्वान्तरात्मा पाण्डुरंगा ;
व्यापक विभु पाण्डुरंगा,
विमला अमला पाण्डुरंगा;
अनादि अनन्ता पाण्डुरंगा,
अजर अविनाशी पाण्डुरंगा ।
आपका नाम एक नाव है पाण्डुरंगा,
इस संसार को पार करने के लिए पाण्डुरंगा
आपका नाम अस्त्र है पाण्डुरंगा,
इस राक्षस मन के नाश के लिए पाण्डुरंगा ।
मैं आपकी दया के लिए दुःखी हूं पाण्डुरंगा,
मैं आपकी कृपा का प्यासा हूँ पाण्डुरंगा।
मुझे अपने मन को लगाने दो पाण्डुरंगा,
आपके चरण-कमलों में पाण्डुरंगा ।
मुझे अपने शरीर का उपयोग करने दो पाण्डुरंगा,
आपकी सदा सेवा में पाण्डुरंगा ।
यह मेरी उत्सुकतापूर्ण प्रार्थना है पाण्डुरंगा,
मत छोड़ना मुझे पाण्डुरंगा ।
आप ही सब कुछ हैं पाण्डुरंगा,
आप सब करने वाले हैं पाण्डुरंगा ।
आप ही वर्तमान हैं पाण्डुरंगा,
आप ही धर्म हैं पाण्डुरंगा ।
आप मेरी आत्मा में रहते हैं पाण्डुरंगा,
आप मेरे पिता हैं पाण्डुरंगा ।
आप मेरे प्राण हैं पाण्डुरंगा,
आप मेरी आत्मा हैं पाण्डुरंगा ।
प्रत्यग चेतना पाण्डुरंगा,
परमार्थ तत्त्व पाण्डुरंगा।
पाण्डुरंगा पाण्डुरंगा,
पाण्डुरंगा पाण्डुरंगा ।
निर्देश गीत
मोहन वंशी वाले तुमको लाखों प्रणाम
तुमको लाखों प्रणाम, करोड़ों प्रणाम
शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम प्यारे करोड़ों प्रणाम ।
भजो राधे गोविन्द,
राधे गोविन्द भजो राधे गोविन्द,
राधे गोवन्द भजो सीता गोविन्द,
हरि बोलो बोलो भाई राधे गोविन्द,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविन्द ।
चार बजे प्रातः जागो ब्रह्ममुहूर्त में,
चार बजे प्रातः उठो जपो राम राम,
चार बजे उठो तुम करो ब्रह्म विचार,
चार बजे उठ कर सोचो 'मैं कौन हूँ?'
चार बजे प्रातः उठो, करो योगाभ्यास ।
नित्य मौन रखो तुम दो घण्टे का,
एकादशी को उपवास करो खाओ फल और दूध,
नित्य अध्याय एक पढ़ो गीता का,
नियमित दान करो कमाई के दसवें भाग का।
अपना काम स्वयं करो नौकरों को त्याग दो,
रात्रि में कीर्तन करो और सत्संग,
सदा सत्य बोलो और रक्षा करो वीर्य की,
सत्यं वद, धर्म चर, करो ब्रह्मचर्य पालन,
अहिंसा परमो धर्मः, सभी से करो प्रेम,
कभी किसी को दुःख न दो, दयालु बनो,
क्रोध को क्षमा से नियन्त्रित करके,
विकसित करो विश्व-प्रेम,
रोज आध्यात्मिक डायरी भरो और करो शीघ्र विकास
(हरे कृष्ण हरे राम ...)
कन्हाई का गीत
कम हीयर माय डियर कृष्ण कन्हाई
मैंने तेरे लिए हृदय अन्दर बिल्डिंग बनाई। (कम हियर...)
तेरे लिए बहुत सारा खाना बनाई,
दूध दही मक्खन मिश्री सारा मँगाई ।
कम सून कम सून कृष्ण कन्हाई, मैंने तेरे.....
रिमेंबरिंग एवरी डे आँसू बहाई,
कम टु माइ हाउस माइ डियर आरती फिराई। (कम हियर...)
तेरे लिए रोज रोज आँसू बहाई, मैंने तेरे....
व्हाय लेट, सो लेट करते कन्हाई,
व्हाय फार, सो फार रहते कन्हाई,
ओ डार्लिंग कन्हाई,
मैंने तेरे लिए हृदय अन्दर बिल्डिंग बनाई। (कम हियर...)
कम हियर, माई डियर, श्याम मुरारी,
प्ले द फ्लूट प्ले द फ्लूट, कुंज बिहारी
फार यू, ओ डियर, 'गोपीज' वेट इन वेन
विद कर्ड, बटर एण्ड मिल्क, हेलिंग यू थ्रो साइन
व्हायरन अवे, रन अवे, डू यू फीयर देम ?
हैव यू स्टोलेन आर हैव यू हिड्डेन एनी प्रेशियस थिंग फ्राम देम?
कम हियर, कम नियर, कृष्ण कन्हाई,
मैंने तेरे लिए हृदय अन्दर बिल्डिंग बनाई। (कम हियर...)
हेल्प द 'गोपीज' एण्ड लोअर द पॉट्स
फ्राम देयर हेड्स सो हाई,
वेयर आर दे, वेयर आर दे, योर 'गोपालाज'?
काल देम आलसो, ब्रिंग देम आलसो,
एण्ड हेल्प गोपिकाज,
कम नियर, क्लोस डियर, 'चोर' मुरारी
टेस्ट द कर्ड, प्ले द फ्लूट, एण्ड डांस, ओ विहारी। (कम हियर...)
कर्मयोगी का गीत
हरि के प्रेमी हरि हरि बोलो,
आओ प्यारे मिल कर गाओ,
हरि चरन में ध्यान लगाओ,
दुख में, सुख में, हरि हरि बोलो,
अभिमान त्यागो, सेवा करो,
नारायण नारायण नारायण नारायण ।
गिव अप ब्राह्मण, संन्यास अभिमान,
गिव अप मेल-फीमेल, सेक्स अभिमान,
गिव अप डाक्टर, जज अभिमान,
गिव अप राजा, जमींदार अभिमान,
रिलिंक्किश पण्डित, साइंटिस्ट अभिमान,
क्रश दिस प्रोफेसर, इंजीनियर अभिमान,
किल दिस कलेक्टर, तहसीलदार अभियान,
किल दिस वैराग्य, सेवा अभिमान,
किल दिस त्यागी, कर्तृत्व अभिमान, (नारायण नारायण...)
रिमेंबर आलवेज हरि हरि हरि
सिंग आलवेज सीताराम राधेश्याम,
सी गाड इन एवरी फेस,
शेयर व्हाट यू हैव विद अदर्स।
डेबलप नाइसली एडाप्टेबिलिटी,
सर्व आलवेज विद नारायण भाव,
स्क्रूटनाइज़ आलवेज योर इनर मोटिव्स,
वर्क विदाउट इगोइजन्म
कल्टिवेट द निमित्त भाव,
गिव अप एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट्स,
सरेंडर आलवेज फ्रूट्स टू द लाई ।
हैव इक्कल विजन एण्ड बेलेन्स्ड माइंड,
सेल्फलेस वर्क विल प्योरीफाइ योर हार्ट,
देन यू विल गेट नालेज ऑफ द सेल्फ । (नारायण नारायण....)
दिव्य जीवन का गीत
गोपाला गोपाला मुरली लोला,
यशोदा नन्दन गोपीबाला ।
सर्व, लव, गिव, प्योरिफाई, प्रेक्टिस अहिंसा,
सत्यम्, ब्रह्मचर्य, टेक सात्त्विक फूड, स्टडी गीता
हैव सत्संग, कन्ट्रोल सेन्सेज, डू जप कीर्तन,
मेडिटेट इन ब्रह्ममुहूर्त, नो दाइ सेल्फ ।
लव आल, एम्ब्रेस आल, बी काइन्ड टू आल,
वर्क इज वर्शिप, (सर्व आल) सर्व द लार्ड इन आल
प्यूरीफाइ, कन्सन्ट्रेट, रिफ्लेक्ट, मेडिटेड,
नो द सेल्फ थ्रू इनक्वारी "हू एम आय ?"
प्यूरीफाइ, कन्सेन्ट्रेट, रिफ्लेक्ट मेडिटेट,
सर्व, लव, गिव एण्ड बी डिस्पैशनेट ;
नो ब्रह्मन, माया, संसार एण्ड "आय" ।
बी होल्ड द गोल ऑफ लाइफ, हे सौम्य नीयर वाइ
(गोपाल गोपाला....)
अमरता का गीत
राम राम राम राम, जय सीता राम,
जय जय राधे श्याम ।
टर्न द गेज, ड्रा द इंद्रियाज़,
स्टिल द माइंड, शार्पेन द इन्टलेक्ट ।
चाँट ॐ विद फीलिंग,
ओ चिल्ड्रन ऑफ लाइट, विल यू ड्रिंक नाट,
बोंट यू ड्रिंक नॉट, द नेक्टर ऑफ इम्मार्टलिटी ?
(राम राम राम राम...)
आल कर्माज़ (आर) बर्नट नाउ,
यू हैव बिकम ए जीवन्मुक्त ।
दैट ब्लेस्ड स्टेट तुरीयावस्था
नो वर्डस् कैन डिस्क्राइव ।
ओ चिल्ड्रन ऑफ लाइट, विल यू ड्रिंक नाट,
वोट यू ड्रिंक नाट, द नेक्टर ऑफ इम्मार्टलिटी ?
(राम राम राम राम...)
द ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड,
एण्ड द स्काई इज ब्लू,
बट द आत्मन इज कलरलेस,
फार्मलेस एण्ड गुणलेस टू ।
ओ चिल्ड्रन आफ लाइट, विल यू ड्रिंक नाट,
वोन्ट यू ड्रिंक नाट, द नेक्टर ऑफ इम्मार्टलिटी ?
(राम राम राम राम...)
लाइफ इज शार्ट, टाइम इज फ्लीटिंग,
द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिसरीज;
कट द नॉट आफ अविद्या
एण्ड ड्रिंक द निर्वाणिक ब्लिस ।
ओ चिल्ड्रन ऑफ लाइट विल यू ड्रिंक नाट,
वॉट यू ड्रिंक नाट, द नेक्टर ऑफ इम्मार्टलिटी ?
(राम राम राम राम...)
फील द डिवाइन प्रेजेंस एवरीवेयर,
सी द डिवाइन ग्लोरी आल एराउण्ड,
देन डाइव डीप इन टू डिवाइन सोर्स,
एण्ड रियलाइज द इनफिनिट ब्लिस।
ओ चिल्ड्रन ऑफ लाइट, बिल यू ड्रिंक नाट
बोट यू ड्रिंक नाट, द नेक्टर ऑफ इम्मार्टलिटी ?
(राम राम राम राम...)
डू आसन, कुम्भक, मुद्रा,
शेक द कुण्डलिनी,
देन टेक इट टू सहस्रार
थ्रू चक्राज इज द सुषुम्ना ।
ओ चिल्ड्रन ऑफ लाइट, बिल यू ड्रिंक नाट,
वोट यू ड्रिंक नाट, द नेक्टर ऑफ इम्मार्टलिटी ?
(राम राम राम राम...)
नारायणम् भजे
नारायणम् भजे नारायणम् भजे,
नारायणम् भजे नारायणम्।
राम राम राम राम राम राम राम राम राम,
राम राम राम राम राम राम राम राम राम ।
रामा कृष्णा हरि, रामा कृष्णा हरि,
रामा कृष्णा हरि, राम राम राम;
राधा कृष्णा हरि, राधा कृष्णा हरि,
राधा कृष्णा हरि, श्याम श्याम श्याम ।
शम्भो सदाशिव शम्भो सदाशिव,
शम्भो सदाशिव, बम बम बम
शम्भो शकर हर, शम्भो शंकर हर,
शम्भो शंकर हर, महादेव ;
गौरी शंकर हर, गौरी शंकर हर, सदाशिवा ।
गौरी शंकर हर, राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी, महेश्वरी;
आदि शक्ति शिव, विष्णु शक्ति हरि, ब्रह्म शक्ति, महा सरस्वती ।
(नारायणम् भजे ...)
निर्गुण
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐ
ॐ सोऽहं शिवोऽहं, सोऽहं शिवोऽहं,
सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् ।
सोऽहं शिवोऽहं, अहं ब्रह्मास्मि,
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मोऽहम् ।
आत्म ब्रह्म स्वरूप, चैतन्य पुरुष,
तेजोमयानन्द तत्-त्वम्-असि लक्ष्य ।
सत्यं शिवं शुभं सुन्दरं कान्त,
सच्चिदानन्द सम्पूर्ण (सुखम् ) शान्तम् ।
प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि,
तत्-त्वम्-असि, अयमात्मा ब्रह्म ।
( ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ...)
नारायण भजे नारायण भजे,
नारायण भजे नारायणम् ।
ॐ का नाद और कीर्तन
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ विचार ॐ ॐ ॐ ॐ भजो
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ कार
( ॐ ॐ ॐ ॐ....)
अगड़ बम गीत
अगड़ बम अगड़ बम बाजे डमरू
नाचे सदाशिव जगत् गुरु
अन्तराय
नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे महादेव
खप्पर लेके काली नाचे नाचे आदि देव;
अगड़ बम अगड़ बम बाजे डमरू
नाचे सदाशिव जगत् गुरु ।
शिव नाम कीर्तन
शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः,
शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय ;
शिव शिव शिव शिव शिवाय नमः,
हर हर हर हर नमः शिवाय ।
शिव शिव शिव शिव शिवाय नमः ॐ
बम बम बम बम नमः शिवाय।
साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव
साम्ब सदाशिव साम्ब शिवाय ।
शिव शिव शंकर हर हर शंकर,
जय जय शंकर नमामि शंकर ।
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः
शिवाय नमः ॐ...)
राजा राम कीर्तन
राजा राम राम राम, सीता राम राम राम
(अन्तराय)
राजा राम राम राम, सीता राम राम राम (राजा राम...)
श्यामा श्याम राधे श्याम, राधा कृष्ण राधे श्याम
(अन्तराय)
राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधा कृष्ण
(राजा राम...)
हे रामा जय रामा, सीता रामा रामा राम
हे रामा जय रामा, सीता रामा रामा राम,
हे रामा जय रामा, रामा सीता रामा रामा।
हे श्यामा जय श्यामा घनश्यामा राधेश्यामा,
हे श्यामा जय श्यामा, घनश्यामा राधेश्यामा,
हे श्याम जय श्यामा, घनश्यामा राधेश्यामा,
हे श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा
घन श्यामा श्यामा राधेश्याम
(राजा राम...)
संकल्प शक्ति के विकास हेतु गीत
भजो राधे कृष्णा, भजो राधे श्यामा,
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
सोऽहं सोऽहं सोऽहं शिवोऽहम्।
विल इज़ आत्म-बल, विल इज डायनेमिक,
हैव ए स्ट्रांग विल एण्ड रियलाइज आत्मा ।
योर विल हैज बिकम वीक, थ्रू वेरियस डिजायरस,
डिस्ट्राय देम टू द रूट बाइ विवेक, वैराग्य, त्याग ।
माई विल इज पावरफुल,
आइ कैन ब्लोअप माउण्टेन्स,
आई कैन स्टाप द ओसीन वेव्स, आई कैन कमाण्ड एलीमेंट्स
आई कैन कमाण्ड नेचर, आई एम वन विद कास्मिक विल,
आई कैन ड्राय अप ओसीन, लाइक मुनि अगस्त्य ।
(भजो राधे कृष्णा, भजो राधे...)
माई विल इज प्योर एण्ड स्ट्रांग, नो वन कैन रेसिस्ट,
आई कैन इन्फ्लूएस पीपल, आई आलवेज गेट सक्सेस ।
आई एम हेल एण्ड हारटी, आई एम आलवेज जायफुल,
आई रेडिएट जाय एण्ड पीस टु मिलियन डिस्टेट फ्रेंड्स ।
आई कैन गिव समाधि बाई सिम्पल गेजिंग,
आई कैन डू शक्ति संचार बाइ मेरा संकल्प,
आई एम योगी ऑफ योगीज, आई एम एम्परर ऑफ एम्परर्स,
आई एम किंग ऑफ आल किंग्स, शाह ऑफ ऑल शाहस ।
आई कैन एलीवेट एस्पिरेंट बाई सिम्पल मास्टर्स टच,
आई कैन वर्क वंडर्स बाई द पावर ऑफ सत्-संकल्प ।
आई कैन वर्क हील मिलियन्स फ्राम ए लांग डिस्टेंस;
दिस इज ड्यू टु विल, देयरफोर डेवलप विल ।
(भजो राधे कृष्णा, भजो राधे...)
गिव अप वासनास एण्ड थिंक ऑफ आत्मा,
दिस इजरायल वे टु डेवलप योर विल ।
कीप अप डायरी, गिव अप केयर्स एण्ड वरीज,
डू सिम्पल तपस् एण्ड डेवलप अटेंशन ।
डेवलप पेशेंश एण्ड हैव कमाण्ड ऑफ टेंपर,
कन्ट्रोल द इन्द्रियास एण्ड प्रेक्टिस मेडिटेशन ।
हैव पावर ऑफ एण्ड्यूरेंस एण्ड प्रेक्टिस सेलीबेसी,
आल दीज विल हेल्प यू टू डेवलप योर विल ।
(भजो राधे कृष्णा, भजो राधे श्यामा...)
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
(भजो राधे कृष्णा, भजो राधे...)
आनन्द का गीत
आनन्दोऽहं आनन्दोऽहं आनन्दं ब्रह्मानन्द
सचराचर परिपूर्ण शिवोऽहं,
सहजानन्द स्वरूप शिवोऽहं,
व्यक्त चेतना आत्म शिवोऽहं,
व्यापक व्यक्त स्वरूप शिवोऽहं,
नित्य शुद्ध निर्मय सोऽह,
नित्यानन्द निरंजन सोऽहं,
अखण्डैकरस चिन्मात्रोऽहं,
भूमानन्द स्वरूप शिवोऽहं,
असंगोऽह अद्वैतोऽहं,
विज्ञानघन चैतन्योऽहं,
निराकार निर्गुण चिन्मयोऽहं,
शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूपोऽहं,
असंग स्वप्रकाश निर्मलोऽहं,
निर्विशेष चिन्मात्र केवलोऽहं,
साक्षी चेतना कूटस्थोऽहं,
नित्य मुक्त स्वरूप शिवोऽहं,
(आनन्दोऽहं आनन्दोऽहं. . . .)
उपनिषद् का गीत
हे रामचन्द्र वृंदावन चन्द्र,
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः,
सर्व व्यापी सर्व अन्तरात्मा,
कर्माध्यक्ष सर्व भूताधिवास,
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।
(एको देवः सर्वभूतेषु गूढः)
सोऽहं शिवोऽहं शिवः केवलोऽह,
शम्भो शंकर, हे महादेव,
गॉड इज वन, ब्रह्म इज वन,
ही इज हिडन इज आल बीइंगस,
लाइक बटर इन मिल्क-लाइक फायर इन वुड,
लाइक माइण्ड इन ब्रेन-लाइक ऑइल इन सीड,
ऑल-परवेडिंग-द सेल्फ ऑफ ऑल बीइंगस।
(एको देवः सर्वभूतेषु गूढः)
सत्येन लभ्य - तपस ही एष आत्मा,
सम्यग ज्ञानेन — ब्रह्मचर्येन नित्यम,
अन्तः शरीरे— ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो,
यं पश्यति यतय— क्षीण दोषः ।
( एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ : )
दिस आत्मन इज एटेंड बाई प्रेक्टिस ऑफ टूथ-तपस,
बाई निर्विकल्प समाधि-बाई प्रेक्टिस ऑफ सेलीबेसी,
इनसाइड द बाडी — रिप्लेन्डेंट प्योर आत्मा,
द एंकोराइट्स बीहोल्ड-हू आर फ्री फ्राम डिफेक्ट्स।
( एको देवः सर्वभूतेषु गूढः)
सत्यं ज्ञान-अनन्त ब्रह्म,
पुरुषोत्तम — परमात्मा,
अदृष्टमं अव्यवहार्यं— अग्राह्यं अलक्षणं,
अचिन्त्यं अव्यापदेश्य – सत्यं अद्वैत ।
( एको देवः सर्वभूतेषु गूढः )
नन्दलाल का गीत
मेरे आँखों में बसो मेरे नन्दलाल
मेरे नन्दलाल प्यारेलाल
मेरे हृदय में बसो मेरे नन्दलाल
रामा रामा हरि सीता राम,
सीता सीता राम, राधे राधे श्याम,
हरि सीता राम, हरि राधे श्याम,
लक्ष्मी नारायण, श्रीमन् नारायण,
हरि ॐ नारायण, बदरीनारायण,
शम्भो शंकर, नमः शिवाय,
(मेरे आँखों में बसो...)
किंडल द लाइट ऑफ लव इन योर हार्ट,
इन्क्लूड आल क्रियेचर्स इन द इम्ब्रेस ऑफ योर लव,
डेवलप कास्मिक लव, शेड टीयर्स ऑफ प्रेम ।
(मेरे आँखों में बसो...)
सोऽहं सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं,
वेक अप फ्राम दिस लाँग ड्रीम ऑफ इलुसरी फार्मस्,
लव योर आत्मन्, लिव इन आत्मन्,
फील द मैजेस्ट्री ऑफ योर ओन इन्नर सेल्फ,
किल इगोइज्म, किल राग-द्वेष,
किल कन्निंगनेस, स्ले क्रूडनेस,
सोऽहं सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं ।
प्रेरक सन्देश और गीत
संगीत रामायण
बाल काण्ड
रामायण कन्टेन्स .................................................. जय जय राम
हायेस्ट डील्स .................................................. सीता राम
ऑफ हिन्दू कल्चर .................................................. जय जय राम
एण्ड सिविलाइजेशन .................................................. सीता राम.
इट इज ए टक्स्ट बुक ऑफ मॉरल्स ..................................... जय जय राम
इट इन्स्पायर द यूथ. . .................................................. सीता राम
द हायर आइडियल्स. .................................................. जय जय राम
ऑफ कंडक्ट एण्ड केरेक्टर................................................... सीता राम
इट कंटेन्ट्स् आब्जेक्ट लेसन्स. .................................................. जय जय राम
फॉर हस्बेंड वाइफ्स . .................................................. सीता राम
फॉर पेरेंट्स, चिल्ड्रन. .................................................. जय जय राम
फार ब्रदर्स एण्ड सिस्टर्स .................................................. सीता राम
इट इज ए मारवलस बुक .................................................. जय जय राम
विच कन्टेन्स द एसेंस .................................................. सीता राम
आफ आल द वेदास .................................................. जय जय राम
एण्ड आल द स्क्रिप्चर्स. .................................................. सीता राम
इट हैज ए मोल्डिंग पावर .................................................. जय जय राम
ऑन द लाइफ आफ मैन .................................................. सीता राम
श्री राम वाज़ बार्न .................................................. जय जय राम
टू डिस्ट्राय रावण .................................................. सीता राम
दशरथ वाज चाइल्डलेस.. ................................................ जय जय राम
ही डिड यज्ञ .................................................. सीता राम
ही हैड श्री वाइफ्स ................................................ जय जय राम
कौशल्या सुमित्रा .................................................. सीता राम
कैकेयी देवी ................................................ जय जय राम
वाज द थर्ड वाइफ .................................................. सीता राम
ही गॉट पायस .................................................. जय जय राम
ही गेव टु हिज बाइफ्स .................................................. सीता राम
द वाइफ्स बिक्रम प्रेग्नेंट . ................................................. जय जय राम
फोर सन्स वेयर बार्न .................................................. सीता राम
राम लक्ष्मण .................................................. जय जय राम
भरत शत्रुघ्न .................................................. सीता राम
ऑल द सन्स .................................................. जय जय राम
वेयर हीरोइक वर्च्युज .................................................. सीता राम
विश्वामित्र. .................................................. जय जय राम
केम टु दशरथ .................................................. सीता राम
ही टुक राम एण्ड लक्ष्मण .................................................. जय जय राम
टु डिस्ट्रॉय द राक्षसाज .................................................. सीता राम
रामा किल्ड .................................................. जय जय राम
ताटका सुबाहु .................................................. सीता राम
रामा थ्रू .................................................. जय जय राम
मारिच इन द ओसीन .................................................. सीता राम
रामा विजिटेड .................................................. जय जय राम
गौतम आश्रम .................................................. सीता राम
टच्ड द स्टोन .................................................. जय जय राम
फ्रीड अहिल्या .................................................. सीता राम
देन रामा वेंट .................................................. जय जय राम
टू मिथिला सिटी .................................................. सीता राम
ही ट्रक द बो .................................................. जय जय राम
बेंट इट इजी .................................................. सीता राम
ही मैरिड .................................................. जय जय राम
द नोबल सीता .................................................. सीता राम
देन ही रिटर्नड .................................................. जय जय राम
टू अयोध्या सिटी .................................................. सीता राम
ऑन द वे .................................................. जय जय राम
ही मेट परशुराम .................................................. सीता राम
ही बेंट हिज बो .................................................. जय जय राम
एण्ड डिफीट हिम. .................................................. सीता राम
राम राम जय . .................................................. सीता राम
राम राम जय .................................................. सीता राम
अयोध्या काण्ड
किंग दशरथ .................................................. जय जय राम
बीकेम ओल्ड .................................................. सीता राम
ही वांटेड .................................................. जय जय राम
टु एन थ्रोन रामा .................................................. सीता राम
आल एरेंजमेन्ट्स .................................................. जय जय राम
वेयर नाइसली मेड .................................................. सीता राम
द क्रुवड मंथरा .................................................. जय जय राम
टोल्ड कैकेयी .................................................. सीता राम
गेट योर टू बून्स .................................................. जय जय राम
फ्राम दशरथ .................................................. सीता राम
बेनिश राम .................................................. जय जय राम
फार फोटॉन ईयर्स .................................................. सीता राम
इन टु दंडक फॉरेस्ट .................................................. जय जय राम
विथ मैटेड लॉक ................................................... सीता राम
एनथ्रोन भरत .................................................. जय जय राम
हैव फ्रीडम कैकेयी .................................................. सीता राम
द क्रूअल कैकेयी .................................................. जय जय राम
आस्कड द टू बून्स .................................................. सीता राम
रामा ओबेड .................................................. जय जय राम
हिज फादर कमाड्स .................................................. सीता राम
ही स्टार्टेड .................................................. जय जय राम
टू द फॉरेस्ट .................................................. सीता राम
लक्ष्मण सीता .................................................. जय जय राम
आलसो फालोड .................................................. सीता राम
ही मेट गुहा .................................................. जय जय राम
किंग ऑफ निषाद .................................................. सीता राम
दे क्रास्ड द रिवर .................................................. जय जय राम
विथ द हेल्प ऑफ गुहा .................................................. सीता राम
देन राम वेंट .................................................. जय जय राम
टु भारद्वाज आश्रम .................................................. सीता राम
देन मार्चड ऑन .................................................. जय जय राम
टू चित्रकूट .................................................. सीता राम
किंग दशरथ .................................................. जय जय राम
गेव अप हिस लाइफ .................................................. सीता राम
ही कुड नाट बियर .................................................. जय जय राम
सेप्रेशन फ्रॉम राम .................................................. सीता राम
मैसेंजर वेयर सेंट .................................................. जय जय राम
टू द नोबल भरत .................................................. सीता राम
ही रिटर्नड .................................................. जय जय राम
फ्रॉम हिज़ अंकल्स पैलेस .................................................. सीता राम
कैकेयी नैरेटेड .................................................. जय जय राम
आल दैट शी डिड .................................................. सीता राम
शी आस्कड भरत .................................................. जय जय राम
टू रूल द किंगडम .................................................. सीता राम
भरत हैड ए .................................................. जय जय राम
टेरेबल शॉक .................................................. सीता राम
ही रिब्यूक्ड .................................................. जय जय राम
हिज़ क्रूअल मदर .................................................. सीता राम
ही एट वन्स स्टार्टेड .................................................. जय जय राम
टू ब्रिंग हिज ब्रदर .................................................. सीता राम
ही रीच्ड स्पीडली .................................................. जय जय राम
द होली चित्रकूट .................................................. सीता राम
द ही रिकेस्टेड राम .................................................. जय जय राम
टु रूल द किंग्डम .................................................. सीता राम
रामा रिफ्यूज्ड .................................................. जय जय राम
टू रूल द किंग्डम .................................................. सीता राम
देन भरत टुक .................................................. जय जय राम
श्री रामाज सैण्डल्स .................................................. सीता राम
भरत लिव्ड .................................................. जय जय राम
इन नन्दीग्राम .................................................. सीता राम
ही रूल्ड द किंगडम .................................................. जय जय राम
जस्टली, वाइसली .................................................. सीता राम
अण्डर द डायरेक्शन .................................................. जय जय राम
ऑफ रामाज सैण्डल्स .................................................. सीता राम
देन रामा वेंट .................................................. जय जय राम
टु अत्रि आश्रम .................................................. सीता राम
अरण्य काण्ड
रामा एण्टर्ड .................................................. जय जय राम
द दंडक फॉरेस्ट .................................................. सीता राम
ही डिस्ट्राय विराध .................................................. जय जय राम
दैट पावरफुल राक्षस .................................................. सीता राम
देन ही मेट .................................................. जय जय राम
शरभंग मुनि .................................................. सीता राम
देयर अपान ही वेंट .................................................. जय जय राम
टु सुतीक्ष्ण आश्रम .................................................. सीता राम
देन ही मेट .................................................. जय जय राम
अगस्त्य मुनि .................................................. सीता राम
अगस्त्य गेव .................................................. जय जय राम
इन्द्राज बो एण्ड एरोज़ .................................................. सीता राम
देन रामा मार्चड .................................................. जय जय राम
टु पंचवटी .................................................. सीता राम
लक्ष्मण कट .................................................. जय जय राम
शूर्पणखाज़ ईयर एण्ड नोज़ .................................................. सीता राम
रामा किल्ड .................................................. जय जय राम
खर एण्ड दूषण .................................................. सीता राम
मरीच एज्यूड .................................................. जय जय राम
द फार्म ऑफ गोल्डन डियर .................................................. सीता राम
सीता टोल्ड रामा .................................................. जय जय राम
लेट मी हैव द डियर .................................................. सीता राम
रामा वेंट आउट .................................................. जय जय राम
टु कैप्चर द डियर .................................................. सीता राम
रावण कैम नाउ .................................................. जय जय राम
टु टेक अवे सीता .................................................. सीता राम
ही पुट ऑन द गुइस .................................................. जय जय राम
ऑफ ए मेडिकेंट .................................................. सीता राम
ही टुक अवे सीता . ................................................. जय जय राम
एण्ड मूव्ड इन द स्काई .................................................. सीता राम
सीता क्राइड .................................................. जय जय राम
राम राम .................................................. सीता राम
जटायु वेंट फोर्थ .................................................. जय जय राम
टु अटैक रावण .................................................. सीता राम
रावण कट .................................................. जय जय राम
जटायुज विंग्स .................................................. सीता राम
सीता टुक हर .................................................. जय जय राम
गारमेंट एण्ड ज्वेल्स .................................................. सीता राम
थ्रूयू देम आन द हिल .................................................. जय जय राम
वेयर द मंकीज़ वेयर सिटिंग .................................................. सीता राम
राव रीच्ड लंका .................................................. जय जय राम
विद जानकी देवी .................................................. सीता राम
ही प्लेस्ड सीता .................................................. जय जय राम
इन अशोक वन .................................................. सीता राम
रामा किल्ड .................................................. जय जय राम
द इलूसिव डियर .................................................. सीता राम
ही कैम बैक विद लक्ष्मण .................................................. जय जय राम
डिड नॉट फाइंड सीता .................................................. सीता राम
रामा सर्चड फार सीता .................................................. जय जय राम
आल ओवर द फॉरेस्ट .................................................. सीता राम
डी मेट जटायु .................................................. जय जय राम
हू 'टोल्ड एवरीथिंग .................................................. सीता राम
रामा ब्लेस्ड .................................................. जय जय राम
द डिवोटेड जटायु .................................................. सीता राम
देन रामा किल्ड .................................................. जय जय राम
द राक्षस कबन्ध .................................................. सीता राम
देन ही मेट .................................................. जय जय राम
द पायस शबरी .................................................. सीता राम
हू टोल्ड रामा .................................................. जय जय राम
टु मीट सुग्रीव .................................................. सीता राम
किष्किन्धा एण्ड सुन्दर काण्ड
देन रामा मेट .................................................. जय जय राम
द माइटी हनुमान .................................................. सीता राम
ही मेड फ्रेंडशिप .................................................. जय जय राम
विद किंग सुग्रीव .................................................. सीता राम
ही किल्ड बाली .................................................. जय जय राम
एण्ड एन्थ्रोन्ड सुग्रीव .................................................. सीता राम
हू आर्डरड मंकीज .................................................. जय जय राम
टु सर्च फॉर सीता .................................................. सीता राम
रामा सेड .................................................. जय जय राम
टु ब्रेव हनुमान .................................................. जय जय राम
गिव दिस रिंग .................................................. जय जय राम
टु बिलब्ड सीत .................................................. सीता राम
मंकीज मेड सर्च .................................................. जय जय राम
बट कुड नाट फाइण्ड सीता .................................................. सीता राम
दे सैट ऑन द सी शोर .................................................. जय जय राम
टु गिव अप देयर लाइफ्स .................................................. सीता राम
सम्पाती केम नाउ .................................................. जय जय राम
एण्ड हेल्पड द मंकीज़ .................................................. सीता राम
ही टोल्ड देम एश्योरली .................................................. जय जय राम
दैट सीता वाज इन लंका .................................................. सीता राम
देन हनुमान क्रास्ड .................................................. जय जय राम
द माइटी ओसीन .................................................. सीता राम
ही डिस्ट्रॉयड लंकिनी .................................................. जय जय राम
ही साँ सीता .................................................. जय जय राम
इन अशोक वन .................................................. सीता राम
ही हैंडेड रामा रिंग .................................................. जय जय राम
टु जानकी देवी .................................................. सीता राम
सीता ही जाइस्ड .................................................. जय जय राम
वेन ही सॉ द रिंग .................................................. सीता राम
सीता गेव हनुमान .................................................. जय जय राम
हर चूड़ामणि .................................................. सीता राम
हनुमान डिस्ट्राड .................................................. जय जय राम
द अशोक वन .................................................. सीता राम
ही रावणस सन .................................................. जय जय राम
अक्षय कुमार .................................................. सीता राम
ही बर्नट .................................................. जय जय राम
द होल ऑफ लंका .................................................. सीता राम
देन ही कम बैक .................................................. जय जय राम
टु रामाज लोटस फीट .................................................. सीता राम
ही गेम टु रामा .................................................. जय जय राम
सीताज चूडामणि .................................................. सीता राम
रामा रोजाइस्ड .................................................. जय जय राम
वेन ही साँ चूडामणि .................................................. सीता राम
युद्ध काण्ड
नल बिल्ट .................................................. जय जय राम
ए ब्यूटीफुल ब्रिज .................................................. सीता राम
द आर्मी ऑफ मंकीज .................................................. जय जय राम
मार्चड टु लंका .................................................. सीता राम
विभीषण केम नाउ .................................................. जय जय राम
ग्लोरियस राम .................................................. सीता राम
ही फेल्स एट हिज़ फीट .................................................. जय जय राम
डिड सेल्फ सरेंडर .................................................. सीता राम
रामा किल्ड .................................................. जय जय राम
कुम्भकर्ण .................................................. सीता राम .
देन केम इन्द्रजित .................................................. जय जय राम
टु फाइट विद राम .................................................. सीता राम
हे सेंट हिज़ अस्त्र .................................................. जय जय राम
टु किल द ब्रदर .................................................. सीता राम
लक्ष्मण फेल डाउन .................................................. जय जय राम
इन एन अनकांशियस स्टेट................................................... सीता राम
हनुमान ब्रॉट ................................................... जय जय राम
संजीवनी बूटी ................................................... सीता राम
लक्ष्मण स्मेल इट .................................................. जय जय राम
एण्ड केम टु सेंसेस .................................................. सीता राम
देन लक्ष्मण किल्ड .................................................. जय जय राम
द माइटी मेघनाद ................................................... सीता राम
रावण केम नाउ .................................................. जय जय राम
टु फाइट विद राम .................................................. सीता राम
रामा सेंट .................................................. जय जय राम
हिज़ ब्रह्म अस्त्र .................................................. सीता राम
रावण फेल डाउन .................................................. जय जय राम
मार्टली वुंडेड .................................................. सीता राम
रामा इन्सटाल्ड .................................................. जय जय राम
विभीषण आन द थ्रोन .................................................. सीता राम
हनुमान टोल्ड सीता .................................................. जय जय राम
ऑफ रामाज़ विक्टरी .................................................. सीता राम
विभीषण ब्राट .................................................. जय जय राम
सीता टु राम .................................................. सीता राम
रामा सस्पेक्टेड .................................................. जय जय राम
सीताज़ कैरेक्टर .................................................. सीता राम
राम राज्य महिमा
सीते वेंट थ्रू .................................................. जय जय राम
द फायर आरडील . ................................................. सीता राम
देन रामा 'एक्सेप्टेड .................................................. जय जय राम
सीता विद जॉय .................................................. सीता राम
देन आल कम बैक .................................................. जय जय राम
टु अयोध्या सिटी ................................................... सीता राम
वसिष्ठ इन्सटाल्ड .. .................................................. जय जय राम
रामा ऑन द थ्रोन .................................................. सीता राम
रामा रूल्ड ................................................... जय जय राम
हिज़ किंगडम जस्टली .................................................. सीता राम
देयर वेयर पीस एण्ड प्लेन्टी .................................................. जय जय राम
एण्ड प्रास्पेरिटी .................................................. सीता राम
हिज रूल वाज़ काल्ड .................................................. जय जय राम
राम राज्य ................................................... सीता राम
ग्लोरी टु वाल्मीकि .................................................. जय जय राम
ग्लोरी टु रामायण .................................................. सीता राम
ग्लोरी टु राम .................................................. जय जय राम
ग्लोरी ट सीता .................................................. सीता राम
मे देयर ब्लेसिंग्स .................................................. जय जय राम
बी अपान यू आल .................................................. सीता राम
ही हू रीड्स .................................................. जय जय राम
संगीत रामायण . ................................................. सीता राम
वेट विद भक्ति .................................................. जय जय राम
एण्ड सेल्फ- सरेंडर .................................................. सीता राम
विद द माइण्ड एण्ड सेन्सेज .................................................. जय जय राम
अण्डर स्ट्रिक्ट कंट्रोल .................................................. सीता राम
प्रेक्टिसिंग सेलीबेसी ................................................... जय जय राम
एण्ड मेडिटेटिंग ऑन राम .................................................. सीता राम
ही विल अटैन .................................................. जय जय राम
सन, वाइफ, वेल्थ .................................................. सीता राम
पीस एण्ड प्लेन्टी . ................................................. जय जय राम
भक्ति मुक्ति .................................................. सीता राम
राम राम राम राम राम राम राम राम ।
राम राम राम राम राम राम राम राम ।
विरह गीत
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे;
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
वेन शैल आइ मीट दी, हे प्रभो,
माय आइज लाँग फार दाइ विज़न;
व्हाई आर्ट तू सो अनकाइण्ड ओ लार्ड !
आइ एम स्लीपलैस ऑल द नाइट।
आइ एम बर्नट द फायर ऑफ विरहा,
दाउ आर्ट मी सोल रिफ्यूजी,
द सीक्रेट एरो ऑफ लव हैज पर्सड माय हार्ट |
(हरे राम ...)
आई कैननॉट सप्रेस मच माइ टीयर्स हाउएवर मच आइ ट्राइ,
दे फ्लो लाइक स्ट्रीम्स एण्ड ड्रेच माइ क्लोथ्स ।
आई फील जॉय इन दाइ रिमेम्बरेंस, हेप्पीनेस इन सिंगिंग
(हरे राम ...)
डूवेल इन भाई आइज हे कृष्णा,
एनथ्रोन इन माई हार्ट श्यामा,
लेट मी हीयर दाइ प्लूट, ओ लार्ड ऑफ वृन्दावन,
माइ हंगर इज़ लोस्ट, माई स्लीप इज गॉन,
माइ माइण्ड इज एवर रेस्टलैस ;
आइ एम वेटिंग आल नाइट टु मीट दी
ओ राधे गोविन्द !
(हरे रामा...)
साँग ऑफ एट्टीन 'इटीज'
(धुन सुना जा सुना जा सुना जा कृष्णा)
सैरेनिटी, रेगुलेरिटी, एवसेन्स ऑफ वेनिटी,
सिन्सिरिटी, सिम्पलीसिटी, वेरेसिटी,
इक्वेनिमिटी, फिक्सिटी, नान इरेटिबिलिटी,
एडाप्टेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, टेनेसिटी,
इन्टेग्रिटी, नोबिलिटी, मैग्नेनिमिटी,
चैरिटी, जेनरोसिटी, प्यूरिटी,
प्रेक्टिस डेली, दीज़, एटटीन 'इटीज़',
यू विल सून अटैन इम्मोटेलिटी,
ब्रह्मन इज द ओनली रीयल एन्टीटी,
यू विल एबाइड इन एटरनिटी एण्ड इनफिनिटी,
यू विल बी होल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
यू कैन नॉट अटैन दिस इन द यूनिवर्सिटी,
(सुना जा सुना जा सुना जा कृष्णा...)
शिवा लोरी
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
सुबह से शाम तक, अंटिल द ब्रेक ऑफ डे,
रिपीट द नेम ऑफ द लार्ड,
राम राम राम राम राम राम
दिस लाइफ इज़ मेंट फार सेल्फ-रियलाइजेशन;
डू रेगुलर संकीर्तन, रीएलाइस द आत्मिक ब्लिस,
डू निष्काम्य कर्म योग,
प्यूरीफाई द हार्ट एण्ड माइण्ड; कन्ट्रोल द इंद्रियाज़,
रेस्ट इन योर ओन स्वरूप ।
वेन यू गेट नॉक्स एण्ड ब्लोज़
इन द डेली बैटल ऑफ लाइफ,
देन द माइण्ड इज़ डली टर्नड टुवर्डस
द स्प्रिचुअल पाथ;
देन कम्स विवेक, वैराग्य,
डिस्पस्ट फार वर्ल्डली थिंग्स,
डिज़ायर फार लिबरेशन, हैव डीप मेडिटेशन।
ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार,
हाउ आई वंडर व्हाट यू आर;
अप एबव द वर्ल्ड सो हाई,
लाइक ए डायमण्ड इन द स्काई।
वेन द ब्लेजिंग सन इज़ सेट,
वेन द ग्रास विद ड्यू इज वेट,
देन यू शो योर लिटल लाइट,
ट्विकल, ट्विंकल आल द नाइट ।
हरि ॐ नारायण, हरि ॐ नारायण,
हरि ॐ नारायण, हरि ॐ नारायण,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।
(राम राम राम...)
ध्यान का गीत
(धुन : लीला, लीला, लीला)
राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम
ट्रुय इस ब्रह्मन, ट्रुथ इज योर ओन सेल्फ;
रियलाइज़ दिस 'ट्रुथ; बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री,
यू मस्ट हैव ए प्योर माइण्ड, इफ यू वांट टु रियलाइज
प्रेक्टिस कर्मयोग, बी प्योर, बी प्योर, बी फ्योर, बी प्योर ।
यू कान्ट एन्जॉय (द) पीस ऑफ माइण्ड
एण्ड कान्ट प्रेक्टिस मेडिटेशन
इफ यू आर पैशनेट;
किल दिस लस्ट, किल दिस लस्ट ।
बी रेगुलर इन योर मेडिटेशन
एण्ड टेक सात्त्विक फूड,
यू विल हैव पीस ऑफ माइण्ड ;
दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ ।
वेन यू मेडिटेट आन हरि,
कीप द पिक्चर इन फ्रन्ट आफ यू,
लुक एट इट विद ए स्टीडी गेज,
यू विल डेवेलोप कन्सन्ट्रेशन ।
इफ इविल थाट्स एन्टर इन योर माइण्ड,
डोन्ट ड्राइव देम फोर्सिबली,
सब्स्टीट्यूर डिवाइन थाट्स,
दे विल पास अवे, दे विल पास अवे ।
मेडिटेशन लीड्स टु नॉलेज,
मेडिटेशन किंल्स पेन्स,
मेडिटेशन ब्रिंग्स पीस;
मेडिटेट, मेडिटेट, मेडिटेट, मेडिटेट ।
समाधि इज यूनियन विद गाड,
दिस फालोज़ मेडिटेशन,
यू विल अटेन इम्पोरटेलिटी
दिस इज मोक्ष, दिस इज मोक्ष ।
(राम राम राम...)
साँग आफ जॉय
विथइन यू इज हिडन गॉड,
विथ इन यू इम्मोर्टल सोल,
किल दिस लिटल आइ,
डाइ टु लिव लीड द डिवाइन लाइफ ।
विथ इन यू इज द फाउन्टेन ऑफ जॉय,
विथइन यू इज द ओसीन ऑफ ब्लिस,
रेस्ट पीसफुली इन योर ओन आत्मन
एण्ड ड्रिंक द नेक्टर ऑफ इम्मोर्टेलिटी ।
सा साधा धा-सा साधा धा
पापा ध प म म म प ग प
ग ग म ग रे स
स स ग म प ध स नि ध प म
ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ- ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ-ॐ ॐ ॐ ॐ
साँग ऑफ एडमोनीशन
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे;
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
इज़ देयर नाट ए नोबलर मिशन,
देन ईटिंग, ड्रिंकिंग एण्ड स्लीपिंग ?
इट इज डिफीकल्ट टु गेट एक हामन बर्थ,
देयर फोर ट्राय योर बेस्ट टु रियलाइज़ इन दिस बर्थ ।
फाइ आन दैट रेच, वो टु दैट मैन,
हू वेस्टस ऑल हिज लाइफ इन सेन्सुअल प्लेजर्स ।
टाइम स्वीप्स अवे, किंग्स एण्ड बेरोन्स,
वेयर इज़ युधिष्ठिर? वेयर इज़ अशोका ?
वेयर इज़ शेक्सपियर ? वेयर इज़ वाल्मीकि ?
वेयर इज नेपोलियन ? वेयर इज शिवाजी ?
बी अप एण्ड डूइंग (इन) योग साधन,
यू बिल एन्जॉय सुप्रीम ब्लिस ।
बी अप एण्ड डूइंग (इन) ब्रह्म विचार,
यू विल अटैन इम्मोर्टलिटी (कैवल्य मोक्ष) ।
(हरे राम हरे राम...)
कैन यू एक्सपैक्ट रीयल शान्ति इफ यू वेस्ट योर टाइम
इन आइडल गासिपिंग ?
कैन यू एन्जॉय सुप्रीम पीस इफ यू वेस्ट योर टाइम
इन नावेल्स (एण्ड) न्यूजपेपरस ?
इन फाइट एण्ड केरल्स ?
इन स्कैंडल एण्ड बैकबाइटिंग ?
(हरे राम हरे राम ...)
एम आई नाट दाउ आर्ट दाउ नाट आई?
वन एलोन इज, देयरफोर टू
वेन न माइण्ड इज मेल्ट इन साइलेंस,
यू विल हैव सेल्फ-रिएलाइजेशन ।
व्हाट यू हैव लर्नट, टेल मी फ्रेंकली फ्राम द
बिहार एण्ट क्वेटा अर्थक्वेक्स ?
हैव यू गाट नाउ रियल वैराग्य ?
डू यू प्रेक्टिस जप एण्ड कीर्तन ?
हीयर इज ए चैलेंज टु नान-बिलीवर ऑफ
द हिन्दू थ्योरी आफ ट्रांसमाइगरेशन ।
हैव यू नॉट द थ्रिलिंग नैरेटिव्स ऑफ
शान्तिदेवी आफ हर पास्ट लाइफ ?
कैन यू एक्सपेक्ट रीयल शान्ति इफ यू वेस्ट योर टाइम
इन कार्डस एण्ड सिनेमाज़ (कार्ड एण्ड स्मोकिंग) ?
वेन योर थ्रोट इज चोक्ड एट द टाइम आफ डेथ
हू विल हेल्प यू फार योर साल्वेशन ?
(हरे राम हरे राम ...)
विभूति योग का गीत
भजो राधे कृष्णा, भजो राधे श्यामा,
भजो राधे कृष्णा, भजो राधे श्यामा।
आई एम नाइदर माइण्ड नॉर बॉडी, इम्मार्टल सेल्फ आइ एम ।
आई एम विटनेस आफ थ्री स्टेट्स,
आइ एम नालेज एबसाल्यूट
आई एम फ्रेमेंस इन जेस्मिन, ब्यूटी इन फ्लावर्स,
आई एम कूलनेस इन द आइस, फ्लेवर इन द काफी।
आई एम ग्रीननेस इन द लीफ,
ह्यू इन द रेनबो,
आई एम टेस्ट बड इन द टंग, ऐसेंस इन आरेंज।
आई एम माइण्ड आफ आल माइंड्स्, प्राण ऑफ आल प्राणस,
आई एम सोल ऑफ आल सोल्स, सेल्फ आफ आल सेल्फ्स ।
आई एम आत्मन ऑफ आल बीइंग्स, एप्पल ऑफ आल आइज़,
आई एम सन ऑफ आल सन्स, लाइट ऑफ आल लाइट्स ।
आई एम प्रणव ऑफ आल वेदास, ब्रह्मन ऑफ उपनिषद्स,
आई एम साइलेंस इन द फारेस्ट, थंडर इन ऑल क्लाउड्स ।
आई एम वेलोसिटी इन इलेक्ट्रान्स, मोशन इन साइंस ।
आई एम इफल्गेन्स इन द सन, वेव इन द रेडियो ।
आई एम सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सोल आफ दिस बॉडी,
आई एम ईयर ऑफ आल इयरस, आई ऑफ आल आइज ।
आई एम टाइम, स्पेस, डिक एण्ड द कन्ट्रोलर,
आई एम गॉड आफ गॉडस, गुरु एण्ड द डायरेक्टर ।
आई एम मेलोडी इन म्यूजिक, इन राग ऐंड रागिनीज,
आई एम साउण्ड इन ईथर, शक्ति इन वीर्य ।
आई एम पावर इन इलेक्ट्रीसिटी, इंटेलिजेंस इन माइण्ड,
आई एम ब्रिलियंस इन फायर, पीनेन्स इन एस्सेटिक्स।
आई एम रीजन इन फिलोसफर्स, विल इन ज्ञानीज़,
आई एम प्रेम इन भक्ताज, समाधि इन योगीज़ ।
आई एम दैट आई एम आई एम, दैट आई एम,
आई एम दैट आई एम आई एम दैट आई एम ।
भजो राधे कृष्णा, भजो राधे श्यामा,
भजो राधे कृष्णा, भजो राधे श्यामा ।
सीता राम कहो
सीता राम कहो, राधे श्याम कहो,
सीता राम कहो, राधे श्याम कहो।
सीता राम बिना सुख सपना नहीं,
राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं।
सीता राम बिना सुख कौन करे,
राधे श्याम बिना दुःख कौन हरे।
सीता राम बिना उद्धार नहीं,
राधे श्याम बिना बेड़ा पार नहीं ।
सीता राम बिना देयर इज नो लाइफ,
राधे श्याम बिना देयर इज नो जॉय ।
सीता राम बिना यू कैन नॉट सी,
राधे श्याम बिना यू कैन नॉट हीयर ।
सीता राम बिना यू कैन नॉट थिंक,
राधे श्याम बिना यू कैन नॉट ब्रीथ ।
सीता राम कहो, राधे श्याम कहो,
सीता राम कहो, राधे श्याम कहो।
वेदान्त का गीत
भजो राधे कृष्णा, भजो राधे श्यामा,
भजो सीता रामा, भजो सिया रामा।
सोऽहं सोऽहं-सोऽहं शिवोऽहं,
ॐ ॐ ॐॐ ॐ- ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
आई एम नाइदर माइण्ड नॉर बॉडी, इम्मार्टल सेल्फ आइ एम,
आई एम विटनेस ऑफ थ्री स्टेट्स,
एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट,
आई एम विटनेस ऑफ थ्री स्टेट्स, नॉलेज एब्सोल्यूट,
आई एम विटनेस ऑफ थ्री स्टेट्स, ब्लिस एब्सोल्यूट ।
आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस बॉडी इज नाट माइन,
आई एम नॉट दिस प्राण, दिस प्राण इज नॉट माइन,
आई एम नॉट दिस माइण्ड, दिस माइण्ड इज नॉट माइन,
आई एम नॉट दिस बुद्धि, दिस बुद्धि इज नॉट माइन,
आई एम दैट आई एम आई एम दैट आई एम,
आई एम दैट आई एम आई एम दैट आई एम ।
आई एम सच्चिदानन्द स्वरूप,
आई एम नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप,
आई एम अकर्ता, आई एम अभोक्ता,
आई एम असंग, आई एम साक्षी ।
प्रज्ञानम् ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि,
तत् त्वम् असि, अयम् आत्मा ब्रह्म,
सत्यम् ज्ञानम् अनन्तम् ब्रह्म,
एकम् एव अद्वितीयम् । भजो राधे कृष्णा,
भजो राधे श्यामा, भजो सीता रामा, भजो सिया रामा।
साँग आफ रीयल साधना
(धुन भैरवी)
डू रियल साधना, माय डियर चिल्ड्रन,
डू रियल साधना
साधना-साधना- साधना-साधना
(डू रियल साधना....
टू फ्री योर सेल्फ फ्राम बर्थ एण्ड डेथ
एण्ड इंज्योय द हायेस्ट ब्लिस,
आई विल टेल यू द श्योरेस्ट वे,
काइंडली हीयरकेन विथ ग्रेटेस्ट
(केयर डू रियल साधना...)
एक्वायर फर्स्ट साधन-चतुष्टय,
देन प्रोसीड टु द फीट ऑफ सद्गुरु,
आफ्टर हैविंग श्रवण एण्ड मनन,
देन डू प्रेक्टिस निदिध्यासन ।
(डू रियल साधना…)
रिमूव फर्स्ट द ओल्ड, ओल्ड देहाध्यास,
बाई रिपीटिंग शिवोऽहं भावना,
देन रिमूव द वेल, आवरण
यू विल रेस्ट इन योर ओन स्वरूप ।
(डू रियल साधना...)
विभिन्न प्रकार के कीर्तन
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश पाहि माम्,
श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश रक्ष माम् ।
जय गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम,
जगद्गुरु परम गुरु सद्गुरु श्याम ।
आदि गुरु अद्वैत गुरु आनन्द गुरु ॐ,
चिद् गुरु चिद्घन गुरु चिन्मय गुरु ॐ ।
बोल शंकर बोल शंकर शंकर शंकर बोल,
हर हर हर हर महादेव शम्भो शंकर बोल ।
ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ,
ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ॐ ।
जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो,
राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो ।
जिस काम में, जिस धाम में, जिस गाँव में रहो,
राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो,
राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो।
राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय हनुमान जय जय हनुमान,
जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम ।
अच्युतं केशवं राम नारायणं,
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम् ;
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं,
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ।
जय राम श्री राधे कृष्ण भज ले सीता राम,
भज ले सीता राम प्यारे भज ले राधे श्याम ।
राधे गोविन्द भजो राधे गोपाल,
राधे गोविन्द भजो राधे गोपाल ।
राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम
नारायणा अच्युता गोविन्दा माधवा केशवा,
सदाशिवा नीलकण्ठा शम्भो शंकरा महादेवा ।
राजेश्वरी माहेश्वरी त्रिपुरा सुन्दरी मातेश्वरी ।
गंगा मैया तार ले पापियों को तार ले।
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या
जीवो ब्रह्मैव नापरः ।
हे कृष्णा आ जा वंशी बजा जा,
हे कृष्णा आ जा गीता सुना जा,
हे कृष्णा आ जा माखन खा जा,
हे कृष्णा आ जा लीला दिखा जा,
अब आ गया बाँसुरी वाला, अब आ गया बाँसुरी वाला ।
आरती गीत
जय जय आरती विघ्न विनायक,
विघ्न विनायक श्री गणेश ।
जय जय आरती सुब्रह्मण्य,
सुब्रह्मण्य कार्तिकेय,
जय जय आरती वेणु गोपाल,
वेणु गोपाल वेणु लोला,
पाप विदूरा नवनित चोरा।
जय जय आरती वेंकटरमण,
जय जय आरती वेंकटरमण,
वेंकटरमण संकटहरण,
सीताराम राधेश्याम ।
जय जय आरती गौरि मनोहर
गौर मनोहर भवानी शंकर,
साम्ब सदाशिव उमामहेश्वर ।
जय जय आरती राजराजेश्वरी,
राजराजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी,
महाकाली महालक्ष्मी,
महासरस्वती महाशक्ति ।
जय जय आरती आंजनेय,
आंजनेय हनुमंत ।
जय जय आरती दत्तात्रेय,
दत्तात्रेय त्रिमूर्ति-अवतार ।
जय जय आरती वेणु गोपाल ।
नोट : ये सभी गीत परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज की आवाज में सीडी और कैसेट में दिव्य जीवन संघ, ऋषिकेश में उपलब्ध हैं।