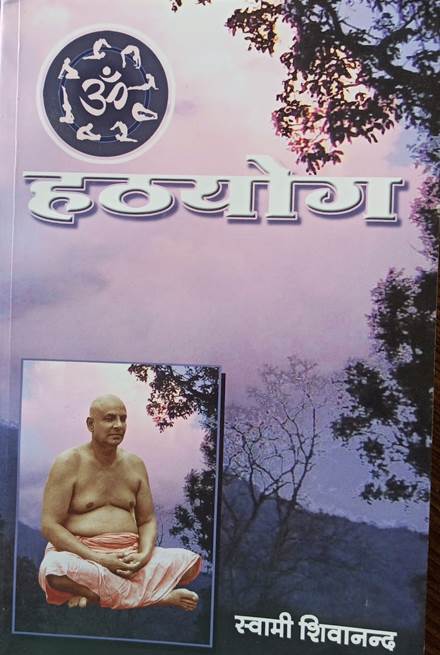
हठयोग
HATHA YOGA का हिन्दी अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती
अनुवादिका
शिवानन्द राधिका अशोक
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर—२४९१९२
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dishq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण : २००७
द्वितीय हिन्दी संस्करण : २०१६
(१००० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
ISBN 81-7052-207-2
HS 4
PRICE : ₹ 100/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए
स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग- वेदान्त
फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर – २४९१९२,
जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित ।
For online orders and Catalogue visit: disbooks.org
प्रकाशकीय
हठयोग किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति हेतु सभी के लिए एक दैवी वरदान है। शरीर एवं मन उपकरण है। ये हठयोग के अभ्यास से दृढ़, शक्तिशाली और ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विरोधी शक्तियों से लड़ने के लिए अस्त्र की भाँति कार्य करते हैं । इसके अभ्यास से आप आदि-व्याधि पर नियन्त्रण कर सकते हैं और उत्तम स्वास्थ्य एवं ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं ।
श्री स्वामी शिवानन्द जी द्वारा लिखी गयी 'हठयोग' पुस्तक उनकी पुस्तक ‘योगासन’ की सहयोगी पुस्तक है । योगासनों के साथ-साथ इसमें प्राणायाम, मुद्राओं, बन्धों और षट्कर्मों का भी विस्तृत एवं सरलता से समझने योग्य विवरण दिया गया है। इसमें 'योग में मूल बन्ध' एवं 'नव 'चक्र विवेक' के बारे में भी बताया गया है। हठयोग जैसा कि यहाँ वर्णित किया गया है, उसे मुख्य रूप से निम्न प्रसिद्ध ग्रन्थों से उद्धृत किया गया है— 'शिव संहिता', 'घेरण्ड संहिता' तथा 'हठयोग प्रदीपिका' । हठयोग के अभ्यास से आपका मन एवं शरीर स्वस्थ रहेगा तथा आपको आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त होंगे ।
'हठयोग' स्वामी जी के बृहत् साहित्य का एक बहुमूल्य रत्न है । हम इस अमूल्य खज़ाने को राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रस्तुत करते हुए आज हर्ष का अनुभव कर रहे हैं और आशा करते हैं कि सभी पाठक गण भी इससे पूर्ण लाभान्वित होंगे ।
-द डिवाइन लाइफ सोसायटी
अनुवादिका का विनम्र निवेदन
यह पुस्तक सन् १९३९ में अंग्रेज़ी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। इस कारण हिंदी भाषी जन अभी तक इससे वंचित थे। गुरुदेव की प्रेरणा से मुझे यह लगा कि इस पुस्तक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना चाहिए; क्योंकि स्वामी जी महाराज ही वे पहले संत थे, जिन्होंने यह बताया कि योग सामान्य जनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है और यह कि इसका अभ्यास मात्र आध्यात्मिक लाभ हेतु ही नहीं, वरन् सांसारिक जीवन में सफल होने के लिए तथा इस शरीर को स्वस्थ रखने हेतु अनिवार्य है। इससे पूर्व योग मात्र हठयोगियों अथवा जिन्होंने इस संसार को तपस्या हेतु त्याग दिया है, के लिए ही उपयोगी माना जाता था। सामान्य मनुष्य इसका अभ्यास करने में भय का अनुभव करता था। किंतु गुरुदेव ने यह भ्रम दूर किया और कहा कि योग से हमारी अंतःशक्तियों का विकास होता है और इस शरीर रूपी उपकरण को स्वस्थ रखने के लिए बच्चे, बड़े, स्त्रियों एवं पुरुषों सभी को योगाभ्यास करना चाहिए। आज जो हम सर्वत्र योग का प्रचार-प्रसार देख रहे हैं, वह स्वामी शिवानंद जी की ही देन है। उन्होंने तीन सौ से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। गुरुदेव कहते थे कि 'मैं मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहता, मैं सभी की आध्यात्मिक मार्ग में सदा सहायता करना चाहता हूँ और मैं इस हेतु अपनी पुस्तकों के रूप में सदा विद्यमान रहूँगा।' गुरुदेव भगवद् साक्षात्कार प्राप्त संत थे, इस कारण उनका लिखा एक-एक शब्द अत्यंत शक्तिशाली है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उनके पास जो भी व्यक्ति आते थे, वे वहाँ आने के पूर्व ही उनकी पुस्तकों को पढ़ कर किसी-न-किसी प्रकार की साधना प्रारंभ कर देते थे। आज भी वे अपनी पुस्तकों के द्वारा जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। 'हठयोग' पुस्तक योग के ऊपर संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। इसमें सभी आवश्यक आसनों, प्राणायामों, बंधों, मुद्राओं, धारणा और ध्यान की विधि आदि का अत्यंत सरल भाषा में वर्णन किया गया है, जिससे वे सरलता पूर्वक सामान्य व्यक्ति को समझ में आ जायें और वे तत्काल योगाभ्यास प्रारंभ कर दें और इसके द्वारा मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इस पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में बताया गया है, वह है नासिका से जल पीना । वास्तव में यह क्रिया अत्यंत लाभदायक है और आशा है कि समस्त हिंदी भाषी जन इस क्रिया का स्वयं अभ्यास कर इसके लाभों का स्वयं साक्षात्कार करेंगे। अंत में सभी पाठकों से विनम्र निवेदन है कि वे इस पुस्तक को मात्र पढ़ें ही नहीं, वरन् इसमें बताये गये आसनों, प्राणायामों आदि का नित्य अभ्यास करें, तो जैसा कि मैंने स्वयं अनुभव किया है, उनके जीवन में भी आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आयेगा।
सदा गुरुदेव की सेवा में,
शिवानन्द राधिका अशोक
शास्त्रों में हठयोग का महत्व
आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः।
इदमेकं सुनिष्पन्नं योगशास्त्रं परं मतम् ॥
(शिवसंहिता)
"सभी शास्त्रों के अध्ययन एवं बार-बार मनन करने पर यह योगशास्त्र ही मात्र सत्य तथा दृढ़ सिद्धांत युक्त पाया गया।”
नास्ति मायासमः पाशो नास्ति योगात्परं बलम् ।
नास्ति ज्ञानात्परो बंधुर्नाहंकारात् परो रिपुः ।
(घेरण्डसंहिता)
"माया के समान कोई बेड़ी नहीं, योग से मिलने वाली शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, ज्ञान के समान श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं और अहंकार के समान "कोई शत्रु नहीं है।"
भ्रांत्या बहुमत ध्वांते राजयोगमजानताम् ।
हठप्रदीपिकां धत्ते स्वात्मारामः कृपाकरः ।।
'अनेक विरोधी मतों के अंधकार में जो भटकते रहते हैं और राजयोग नहीं प्राप्त कर पाते, उनके लिए सर्व कृपालु स्वात्माराम योगी हठयोग का प्रकाश प्रदान करते हैं।"
अशेषतापतप्तानां समाश्रयमठो हठः।
अशेषयोगयुक्तानामाधारकमठो हठः ।।
"जो त्रितापों से जलाये जा रहे हैं, उनके लिए हठयोग मंदिर के समान है तथा जो योगाभ्यास में लगे हैं, उन सभी के लिए हठयोग उस कच्छप के समान है जो इस संपूर्ण जगत का आधार है।"
युवा वृद्धोऽतिवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा ।
अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेष्वतंद्रितः ॥
(हठयोगप्रदीपिका)
"यदि कोई लगन पूर्वक योगाभ्यास करता है, तो चाहे वह युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, रोगी अथवा दुर्बल क्यों न हो, सिद्ध बन जाता है।"
प्रस्तावना
बृहत सूर्य से ले कर छोटे से अणु तक यह संपूर्ण विश्व नियम द्वारा नियंत्रित है। सर्वत्र एक निश्चित नियम है। सूर्य अपना काम पूर्ण नियमितता से करता है। यह सही समय पर उदित होता है और सही समय पर अस्त हो जाता है। तारे और ग्रह एक निश्चित क्रम में भ्रमण करते हैं। ये सभी एक नियम द्वारा नियंत्रित हैं। मनस लोक में भी नियम हैं। भौतिकी, खगोल शास्त्र, गणित सभी के नियम हैं। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियम हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इस बृहत विश्व में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो सभी नियमों को तोड़ता है और इनका उल्लंघन करता है। नियम विरुद्धता एवं नियम त्यागने का मनुष्य एकमात्र उदाहरण है। वह स्वास्थ्य के नियमों का पूर्ण उल्लंघन करता है, अनैतिक जीवन व्यतीत करता है और फिर आश्चर्य करता है कि वह रोगों तथा असंगति से पीड़ित क्यों है। वह स्वच्छता एवं उचित जीवन के नियमों की पूर्ण उपेक्षा करता है और फिर जब वह किसी भयंकर असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है, तो रोता है।
वह चीज क्या है जो जीवन को बहुमूल्य बनाती है? वह है स्वास्थ्य "शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम् " मानव अस्तित्व के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर वास्तव में एक अनिवार्य साधन है।
चरक महर्षि ने अपनी संहिता में लिखा है: “धर्मार्थ काम मोक्षानाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम्, योगस्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितायच”—गुणों, धन, कामना, मुक्ति एवं आनंद हेतु उत्तम स्वास्थ्य सहायक है। रोग स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। स्वास्थ्य संरक्षण के नियमों का ध्यान रखना सर्वाधिक आवश्यक है। स्वास्थ्य संरक्षण के नियम प्रकृति के नियम हैं। इनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिये। जो इन नियमों की अवहेलना करते हैं, वे असाध्य रोगों का शिकार हो जाते हैं।
स्वास्थ्य ही संपत्ति है। स्वास्थ्य ही वास्तव में ऐसी संपत्ति है जिसका लोभ किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सभी के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति है। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य वह स्थिति है, जिसमें मनुष्य अच्छी नींद सोता है, उसका भोजन अच्छी तरह पचता है तथा वह सभी रोगों से मुक्त रहता | जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो सभी अंग जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, वृक्क, यकृत, आँतें आदि समन्वय पूर्वक तथा संतोष जनक ढंग से कार्य करते हैं और नाड़ी की गति सही रहती है, शरीर का तापमान सामान्य रहता है एवं नित्य खुल कर शौच होता है। स्वस्थ मनुष्य सदा मुस्कुराता और हँसता रहता है। वह सदा उत्साहित रहता है। वह अपने नित्य कर्तव्य अत्यंत सहज रूप से करता है। स्वस्थ मनुष्य बिना थके लंबे समय तक कार्य कर सकता है। उसके पास श्रेष्ठ मानसिक एवं शारीरिक क्षमता होती है।
स्वस्थ मनुष्य आवश्यक नहीं कि बलवान् हो, और बलवान् मनुष्य आवश्यक नहीं कि स्वस्थ हो । अत्यंत बलवान् व्यक्ति हो सकता है रोगों से पीड़ित हो । स्वस्थ तथा बलवान् व्यक्ति सबके आकर्षण का केंद्र होता है। वह जिनके भी संपर्क में आता है, उन सभी में स्वास्थ्य एवं शक्ति का विकिरण करता है। शक्ति एवं आकार के द्वारा आप उसके स्वास्थ्य का अनुमान नहीं लगा सकते। एक दुबला-पतला अथवा भारी शरीर वाला व्यक्ति भी बलवान् हो सकता है। आपके भीतर माँसपेशियों की शक्ति के साथ-साथ नाड़ी शक्ति भी होनी चाहिए। शक्तियाँ भी विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ लोग भारी वजन उठा सकते हैं। कुछ लोग अत्यधिक गर्मी तथा शीत को सहन कर सकते हैं। कुछ लोग कई दिनों तक उपवास रख सकते हैं। कुछ अपमान तथा आघात सहन कर सकते हैं। कुछ कार को रोक सकते हैं और जंजीरें तोड़ सकते हैं। कुछ लोग लंबी दूरी तक तैर सकते हैं। कई लोगों के पास बहुत अधिक शारीरिक शक्ति होती है, किंतु उनके पास मानसिक शक्ति नहीं होती। एक कठोर शब्द उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। कुछ लोग प्रचुर शक्ति संपन्न होते हैं, लेकिन वे किसी तीव्र रोग का दर्द सहन नहीं कर सकते। जब वे किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तो बच्चों की तरह बिलखने लगते हैं। उनके पास थोड़ी सी भी मानसिक शक्ति नहीं होती। कुछ लोग शारीरिक रूप से बलवान् होते हुए भी लोगों की आलोचना से डरते हैं।
जिसके पास शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति है, वह एक आदर्श व्यक्ति है। नैतिक बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक शक्ति पृथ्वी पर सर्वोच्च शक्ति है। वह संत अथवा योगी जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, वह संपूर्ण जगत् को चला सकता है। उसका व्यक्तित्व अद्भुत होता है। गाँधी जी के पास नैतिक शक्ति थी। उन्होंने यह शक्ति अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के अभ्यास से अर्जित की थी। गाँधी के पास शारीरिक बल तो नहीं था, लेकिन उनके पास मानसिक और आध्यात्मिक बल था। दुबले-पतले शरीर में भी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आत्मा निवास कर सकती है।
आज संसार को अच्छी स्वस्थ माताओं, शक्तिशाली बालकों तथा बालिकाओं की आवश्यकता है। भारत वह भूमि है, जिसने भीष्म, भीम, अर्जुन, द्रोण, अश्वत्थामा, कृप, परशुराम तथा असंख्य पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। वह भूमि जहाँ के असंख्य राजपूत निस्संदेह रूप से निर्भीकता, अतुलनीय शक्ति एवं पराक्रम से सम्पन्न रहे हैं, आज उसी भारत में आप क्या पाते हैं ? आज वहाँ के लोग दुर्बल तथा नपुंसक हो गये हैं। बच्चे बच्चों को जन्म दे रहे हैं। स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना, उपेक्षा हो रही है। देश मर रहा है, पीड़ित है । आज जगत को पराक्रमी, नैतिक और आध्यात्मिक ऐसे अनगिनत सैनिकों की आवश्यकता है जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से संपन्न हो। जिनके पास स्वास्थ्य और शक्ति है तथा जिनके पास उपरोक्त पाँचों सद्गुण हैं, जिनके पास आत्मज्ञान है, वे ही जगत हेतु सच्ची स्वतंत्रता सुरक्षित कर सकते हैं।
उत्तम स्वास्थ्य आपकी महान् धरोहर है। बिना उत्तम स्वास्थ्य के आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलना कठिन है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक लक्ष्य हेतु भी उत्तम स्वास्थ्य पूर्वापेक्षा है। बिना उत्तम स्वास्थ्य के आप अपने अंतर के जीवन के बृहत सागर की गहराइयों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और न ही जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उत्तम स्वास्थ्य के बिना आप उपद्रवी इंद्रियों तथा प्रबल मन से संघर्ष नहीं कर सकेंगे।
शुद्ध जल पीने से, शुद्ध पौष्टिक भोजन ग्रहण करने से, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियमों का पालन करने से, नियमित व्यायाम करने से तथा प्रातः काल शीतल जल से स्नान करने से, जप तथा ध्यान का अभ्यास करने से, सही जीवन जीने से, सही सोच रखने से, अच्छे कार्य करने से, सही आचरण से, ब्रह्मचर्य के पालन से, नित्य कुछ देर खुली हवा तथा सूर्य के प्रकाश में निवास करने से आपको अद्भुत स्वास्थ्य, बल और जीवनी शक्ति प्राप्त होगी।
सात्विक आहार अथवा अच्छा पौष्टिक आहार एवं पूर्ण आहार लेना, योगासनों का नियमित क्रमबद्ध अभ्यास, सही जीवन जीना, सही सोच रखना तथा सादा जीवन व्यतीत करना, ये सभी उच्च स्तरीय बल तथा जीवनी शक्ति प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षायें हैं। ये सभी वे उत्कृष्ट सिद्धांत हैं, जिनका पालन कर प्राचीन ऋषि और योगी दीर्घायु रहते थे तथा शांति पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, ये सभी वे महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, जिन पर योगका तंत्र आधारित है और इनसे शरीर एवं मन के स्वास्थ्य में पूर्णता की प्राप्ति होती है। ये वे आधार हैं, जिनसे भारत देश अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त कर सकता है।
यदि यौगिक क्रियाओं का नित्य १५ मिनट अभ्यास किया जाये तो आप पूर्ण स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रहेंगे। आपमें प्रचुर ऊर्जा, पेशी बल तथा नाड़ी शक्ति होगी। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा तथा आप दीर्घायु
आजकल अनेक प्रकार की व्यायाम की विधियाँ प्रचलित हैं, उनमें से हटयोग श्रेष्ठ है। प्राचीन ऋषियों एवं योगियों ने इसका अभ्यास किया था। यह सर्वाधिक त्रुटि रहित विधि है। इससे मस्तिष्क, माँसपेशियाँ, नाड़ियाँ, शरीर के अंग, ऊतक आदि की मालिश होती है और शक्ति प्राप्त होती है। सभी जीर्ण रोग जड़ से दूर हो जाते हैं। हठयोग की क्रियाओं के अभ्यास से आपको स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन प्राप्त होता है तथा आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। हठयोग में क्रियाओं का क्रमबद्ध अभ्यास आता है। इसमें षट्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध तथा ध्यान एवं धारणा की क्रियायें सनिहित हैं।
आसन भौतिक शरीर से सम्बद्ध हैं। ये शरीर को दृढ़ एवं स्थिर रखते हैं। बंध प्राण से सम्बद्ध हैं। जो बाँधता है, वह बंध है। ये प्राण को ऊपर नहीं जाने देते और अपान को नीचे नहीं जाने देते। ये प्राण तथा अपान को बाँधते हैं, मिलाते हैं तथा इस संयुक्त प्राण और अपान को सुषुम्ना के साथ भेजते हैं। मुद्रायें मन के साथ संबद्ध हैं। ये आत्मा के साथ मन को बंद कर देती हैं। ये मन को विषयों की ओर नहीं भागने देतीं। ये बहिर्गामी मन को हृदय गुहा में आत्मा की ओर निर्दिष्ट करती हैं तथा इसे वहाँ स्थिर करती हैं। किंतु सभी क्रियाओं का संयुक्त अभ्यास आवश्यक है।
इस पुस्तक का प्रथम अध्याय प्रमुख आसनों के बारे में व्यवहृत है। स्वास्थ्य तथा शक्ति के लिए मैंने २० आसनों का वर्णन किया है। आसनों की प्रकृति एवं लाभ के अनुसार ये ८ समूहों में विभाजित किये गये हैं। ८ वें समूह में ध्यान हेतु सर्वश्रेष्ठ ४ आसनों का वर्णन किया गया है। अध्याय २ में प्राणायाम की विधियाँ वर्णित हैं। प्राणायाम के अभ्यास से फेफड़ों में रक्त परिसंचरण में वृद्धि होती है और नाड़ियों की शुद्धि होती है।
तीसरे अध्याय में आपको मुद्राओं तथा बंधों की जानकारी मिलेगी। अंत में मैंने कुंडलिनी, इसके जागरण, धारणा, स्वास्थ्य तथा दीर्घायु के बारे में महत्वपूर्ण लेख दिये हैं। इसके पश्चात् आपको नित्य अभ्यास हेतु आसनों का समूह दिया गया है। प्रत्येक समूह से आपको अपने स्वभाव, क्षमता एवं उपलब्ध समय के अनुसार एक या दो आसन चुन लेने चाहिए। यदि आप प्रत्येक समूह से एक आसन भी चुन लें तथा प्रतिदिन १५ मिनट भी इसका अभ्यास करें, तो भी आपके शरीर का सम्पूर्ण विकास होगा।
आप सभी को योगाभ्यास एवं ऋषियों के आशीर्वाद से उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, उच्चस्तरीय बल तथा जीवनी शक्ति प्राप्त हो!
-स्वामी शिवानंद
प्रार्थना
हे देवी माँ, हे सर्पिणी कुंडलिनी शक्ति !
हमारे हृदय में वास करने वाली !
आप साढ़े तीन कुंडल मारे हुए, मूलाधार में सोई हुई हैं।
आप ही साकार और निराकार हैं।
आप ही सगुण और निर्गुण हैं।
आप ही स्रोत और अवलंबन हैं।
आप कण-कण में विद्यमान हैं।
वेद आपका गुणगान करते हैं।
संत आप पर ध्यान करते हैं।
योगी आपका ध्यान करते हैं।
भक्त आपकी पूजा करते हैं।
आप गहन हैं।
आप अबोधगम्य है।
आप अविचल हैं।
आप अचिंतनीय हैं।
भक्त आपकी पूजा करते हैं।
हमारे नेत्र आपको ही देखें।
अब हमारी जिहा आपका ही गुणगान करे।
अब हमारे हाथ आपके ही लिए कार्य करें।
अब हमारे मन आप पर ही द्रढ़ रहें।
अब मैं सहस्रार में ही लीन रहूँ ।
अब मेरी सुषुम्ना का द्वार खुल जाये ।
अब मेरी कुंडलिनी जाग्रत हो जाये।
अब मैं हठयोग के अमृत का पान करूँ
अब मैं समाधि प्राप्त करूँ।
अब मेरे प्राण अपान के साथ एक हो जायें।
अब मुझे केवल कुंभक प्राप्त हो, और मुझे आपके साथ एक होने दें।
हठयोग की महिमा
भैया, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करो,
स्वास्थ्य के बिना तुम कैसे जियोगे ?
स्वास्थ्य के बिना कैसे अर्जन करोगे?
स्वास्थ्य के बिना तुम कैसे आगे बढ़ोगे?
हठयोग से स्वास्थ्य प्राप्त करके,
ह का ठ से मिलन करके,
चंद्रमा का सूर्य के साथ मिलन करके,
प्राण का अपान के साथ मिलन करके,
सहस्रार में अमृत का पान करो,
और अमर धाम में निवास करो,
हठ एवं राजयोग अभिन्न हैं,
जहाँ हठयोग समाप्त होता है,
वहाँ राजयोग प्रारंभ होता है।
हठयोग आपको निर्विकल्प समाधि लिए तैयार करता है।
हठयोग के बिना सफलता नहीं,
हठयोग के बिना समाधि नहीं,
हठयोग के बिना वीर्य नहीं,
हठयोग के बिना स्वास्थ्य नहीं,
हठयोग के बिना सौंदर्य नहीं,
हठयोग के बिना दीर्घायु नहीं,
अभ्यास आरंभ करने के पहले गणेश जी को प्रणाम करें,
आसनों के राजा शीर्षासन का अभ्यास करें और
सभी रोगों को दूर करें,
सर्वांग आसन के अभ्यास से थायराइड ग्रंथि का विकास करें,
और पश्चिमोत्तानासन द्वारा
भोजन का पाचन करें,
मयूरासन से विष भी पच जाता है।
अर्ध मत्स्येंद्र आसन रीढ़ को लचीली बनाता है।
भुजंग, शलभ और धनुर आसन के अभ्यास से
शौच खुल कर होता है।
तथा ये कब्ज को समूल नष्ट कर देते हैं।
शीर्ष, सर्वांग आसन द्वारा वीर्य का संरक्षण करें
और स्वप्न दोष से बचें।
शवासन में माँसपेशियों को
विश्राम प्रदान करें।
आगे झुकने और पीछे मुड़ने वाले
आसनों की उपेक्षा न करें,
यदि आप चहुंमुखी विकास चाहते हैं,
तो रीढ़ को मोड़ने की उपेक्षा न करें।
पश्चिमोत्तानासन से पेट की चर्बी कम होती है।
हलासन से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है।
वज्रासन से आलस्य निश्चित रूप से दूर होता है,
और मत्स्यासन से सर्वांग आसन के प्रभाव में वृद्धि होती है।
प्राणायाम से सभी रोग दूर होते हैं
एवं जठराग्नि में वृद्धि होती है।
हलका सा कुंभक दीर्घायु तथा शक्ति
स्फूर्ति एवं जीवनी शक्ति प्रदान करेगा
और कुंडलिनी का जागरण करेगा।
शीतली मस्तिष्क एवं शरीर को शीतल करता है,
तथा रक्त को शुद्ध करता है।
भस्त्रिका अस्थमा और कब्ज को दूर करेगा।
बंध त्रय आपको सुंदर बना सकता है।
प्रातःकाल अभ्यास हेतु अति अनुकूल है।
आसन से प्रारंभ करें, फिर प्राणायाम करें।
प्रतिदिन आसन, प्राणायाम हेतु १५ मिनट व्यय करें।
यह आपको स्वस्थ रखने हेतु पर्याप्त है।
अपने अभ्यास में नियमित रहें,
अंत में थोड़ा दूध पिएं,
स्नान हेतु १ घंटे प्रतीक्षा करें।
भोजन एवं निद्रा में संयमित रहें।
गर्म कढ़ी, प्याज का त्याग करें।
आसनों का अभ्यास खाली पेट करें।
विषय-सूची
समूह १ : सिर के बल किये जाने वाले आसन
समूह २ : शरीर को आगे की ओर मोड़ने वाले आसन
समूह ३ : शरीर को पीछे की ओर मोड़ने वाले आसन
समूह ४ : बगल की ओर झुकने वाले आसन
समूह ५ : मेरुदंड को मोड़ने वाले आसन
२. कुंडलिनी का जागरण कैसे करें?
५. ब्रह्मचर्य द्वारा जीवन में वृद्धि
शरीर के संपूर्ण विकास के लिए आसन
बीस महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक नियम
अध्याय १
आसन
समूह १ : सिर के बल किये जाने वाले आसन
१. शीर्षासन
शीर्षासन सभी आसनों का राजा है। इस आसन के अभ्यास से आपको अधिकतम शारीरिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होंगे। संस्कृत में 'शीर्ष' का अर्थ है सिर। चूँकि इस आसन में अभ्यासी सिर के बल खड़ा रहता है, इस कारण इसे शीर्षासन कहते हैं। इसका अन्य नाम कपाली आसन है (कपाल अर्थात सिर)।
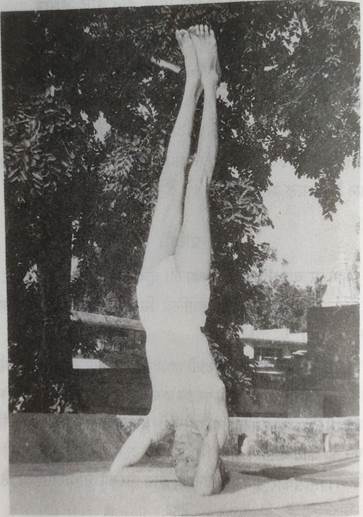
प्रविधि
भूमि पर चारवर्ती कंबल बिछा लें। चूंकि इस आसन में सारे शरीर का भार सिर के ऊपर रहता है, इसलिये सिर के नीचे कंबल का होना आवश्यक है।
घुटनों के बल बैठ जायें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। फंसी हुई उंगलियों को भूमि पर इस प्रकार रखें कि हाथ सिर के शीर्ष भाग के पास रहें इस समय कोहनियाँ सारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिये आधार का कार्य करेंगी। निम्न चित्र के द्वारा आप देख सकेंगे कि फंसी हुई उंगलियाँ किस प्रकार भूमि पर रखनी हैं, इनसे सिर को आधार मिलता है।
अब अपने सिर का शीर्ष भाग हाथों के बीच रखें और उंगलियों को फंसा लें। शरीर को ऊपर उठायें और घुटनों को अपने सीने के पास लायें ।
पंजे भूमि को स्पर्श करेंगे, इस स्थिति से आपको धीरे-धीरे पंजों को भूमि से ऊपर उठाने का प्रयत्न करना है २, ३ बार में आप शरीर को संतुलित करने की कला सीख जायेंगे। आप दीवार के सहारे इस आसन को सफलता पूर्वक सीख सकेंगे। हाथों और सिर को दीवार के पास रखें और अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर की ओर ले कर जायें। अपने पैरों को दीवार से दूर करने का प्रयास करें। इस विधि से आप शरीर को संतुलित करने की विधि सीख सकेंगे। आप अपने मित्र से भी अपने पैरों को पकड़ने के लिए कह सकते हैं। यह देखने के लिए कि आप स्वयं स्थिर रह सकते हैं या नहीं, वह आपके पैरों को कभी-कभी छोड़ भी सकता है।
जब आप आसन में रुके हों, तो सदा नासिका से श्वाँस लें, कभी भी मुँह से श्वाँस न लें। कुछ दिनों तक आपको नासिका से श्वाँस लेने में कष्ट का अनुभव होगा, फिर आपको सरल लगने लगेगा।
यदि आपको इस प्रकार कठिनाई का अनुभव हो तो आप हथेलियों को भूमि पर भी रख सकते हैं। कुछ समय बाद आप पूर्व वाली विधि अपना सकते हैं। आसन के समाप्त हो जाने पर आप थोड़ी देर तक सीधे खड़े रहें। और अगला आसन प्रारंभ करने के पहले कुछ देर विश्राम करें। ऐसा करने से आपका रक्त संचरण सही रहेगा। कुछ लोग इस आसन में एक साथ तीन घंटे तक रुक सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इस आसन को अधिक लंबे समय तक न करें। जब आप आसन कर रहे हों तो इष्ट मंत्र का जप भी कर सकते हैं।
लाभ
इस आसन में सम्पूर्ण शरीर उल्टा हो जाता है, इस कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण महाधमनी, गले की धमनी, अनुजत्रिक धर्मनी आदि शुद्ध रक्त से भर जाती हैं। मात्र इसी आसन में मस्तिष्क को शुद्ध रक्त की आपूर्ति होती है। बारह जोड़ी कपालीय नाड़ियों, मेरुरज्जु, ३१ जोड़ी मेरु नाड़ियों तथा संवेदी तंत्र को पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है। नाड़ियों, नेत्रों, नासिका, गले तथा कानों के समस्त दोष इस आसन के अभ्यास से दूर हो जाते हैं। यह एक शक्तिशाली नाड़ी शक्ति प्रदायक इससे संपूर्ण नाड़ी तंत्र की मालिश होती है एवं पोषण मिलता है। सभी शिराओं का रक्त चूँकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है, इसलिए उनको गुरुत्वाकर्षण बल से सहायता मिलती है। और शिराओं तथा उनके कपाटों को विश्राम प्राप्त होता है। इसी कारण यह वेरीकोज वेन्स रोग के उपचार में सहायता करता है।
यह ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहायक है। इससे वीर्य शक्ति ओज़ में परिणित हो जाती है और मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होती है, इस ओज़ शक्ति का उपयोग ध्यान हेतु होता है। इसे यौन शुद्धिकरण भी कहते हैं। स्वप्न दोष से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से बड़ा आराम मिलता है। शीर्षासन के उपरांत ध्यान करने से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इस आसन में आप अनाहत नाद स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं।
शीर्षासन शक्ति में वृद्धि करता और जीवन देता है। यह सभी रोगों की राम बाण औषधि है। यह शक्तिशाली रक्त शोधक है। इसके अभ्यास से झुर्रियाँ तथा सफेद बाल अदृश्य हो जाते हैं। यह यकृत, प्लीहा, फेफड़ों तथा जननांगों एवं उत्सर्जक अंगों से सम्बंधित समस्त रोगों को दूर करता है। यह बहरापन, मधुमेह, बवासीर, पायरिया, कब्ज आदि रोगों को दूर करता है। इससे पाचन शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है। यह स्त्रियों के लिए भी अति उत्तम है। किंतु मासिक धर्म एवं गर्भधारण के समय इसे करना ठीक नहीं है। इसके अभ्यास से नपुंसकता समाप्त हो जाती है तथा स्मरण शक्ति में अद्भुत रूप से वृद्धि होती है। वकीलों, विचारकों ने इसे बड़ा उपयोगी पाया है। इसको करते समय यदि आप श्वाँस पर ध्यान देंगे तो पायेंगे कि यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जा रही है। यह आसन स्वाभाविक रूप से प्राणायाम हेतु प्रेरित करता है और यह मूलाधार में स्थित कुंडलिनी के जागरण करता है।
२. ऊर्ध्व पद्मासन
यदि आप शीर्षासन अच्छी तरह से कर सकते और इसमें अपने शरीर का संतुलन बनाये रख सकते हैं, तो आप ऊर्ध्व पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप शीर्षासन में खड़े हों, तब धीरे से बायें पैर को मोड़ें और दाँय जाँघ पर रख दें, इसी प्रकार दायें पैर को मोड़ें और बाँय जाँघ पर रख दें। इस प्रकार पद्मासन बन जायेगा ।
यदि आप बैठ कर पद्मासन कर सकते हैं तो आप ऊर्ध्व पद्मासन हेतु प्रयत्न कर सकते हैं। आपको यह आसन अत्यंत सावधानी पूर्वक तथा धीरे-धीरे करना चाहिए। वह व्यायामी जो पैरेलल बार अथवा भूमि पर संतुलन कर सकता है, वह इस आसन को सरलता से कर सकता है। प्रारंभ में इस आसन में १५ सेकेंड तक रुकें, फिर पद्मासन को खोल दें। इसके बाद कुछ सेकेंड तक शीर्षासन में रुकें, फिर धीरे-धीरे पैरों को नीचे लायें। जैसा कि शीर्षासन में पूर्व में निर्देश दिया गया है, आसन समाप्त होने पर थोड़ी देर तक सीधे खड़े रहें। इससे रक्त का परिसंचरण संतुलित हो जायेगा। शीर्षासन के सभी लाभ इससे प्राप्त होते हैं। जो इसका अभ्यास करता है, उसका शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रहता है।
३. सर्वांग आसन
सर्वांग का अर्थ है-सभी अंग। यह नाम बतलाता है कि यह सभी अंगों से सम्बद्ध है। यह एक अनूठा आसन है जो कि संपूर्ण शरीर को नवजीवन प्रदान करता है।
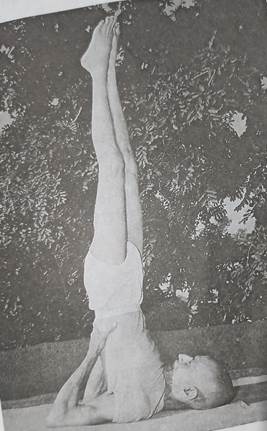
प्रविधि
भूमि पर मोटा कंबल बिछा लें। पीठ के बल लेट जायें। धीरे-धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठायें। पेट, जाँघ तथा पैरों को बिल्कुल सीधे उठायें। कोहनियों को भूमि पर दृढ़ता से लगाये रखें और पीठ को दोनों हाथों से सहारा दें। पैरों को तब तक उठायें जब तक कि वे सीधे लम्बवत न हो जायें। ठोड़ी से सीने पर दबाव दें। यह जालंधर बंध है। जब आप यह आसन कर रहे हों, तो आपकी गर्दन, सिर का पिछला भाग और कंधे भूमि को स्पर्श करने चाहिये। धीरे-धीरे श्वाँस लें तथा गले में स्थित थायराइड ग्रंथि का ध्यान करें। शरीर को आगे-पीछे न जाने दें। जब आसन समाप्त हो जाये तो पैरों को बड़ी सावधानी से धीरे-धीरे नीचे लायें, झटका नहीं लगना चाहिए। आसन को अत्यंत सुंदर ढंग से करें। इस आसन में आप हाथों के सहारे खड़े रहते हैं। और आपका सम्पूर्ण भार कंधों पर रहता है। इसके तुरंत बाद मत्स्यासन का अभ्यास करना चाहिए जिससे आप सर्वांग आसन के अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस आसन में प्रारंभ में मात्र दो ही मिनट रुकें, फिर इस अवधि को धीरे-धीरे ३० मिनट तक बढ़ायें।
लाभ
जिस प्रकार शीर्षासन संपूर्ण तंत्रिका तंत्र की मालिश करता है, उसी प्रकार सर्वांग आसन (अवटु ग्रंथि) थायराइड ग्रंथि का विकास करके संपूर्ण शरीर तथा इसके कार्यों में सहयोग करता है। अवटु (थायराइड) ग्रंथि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इस आसन में इस ग्रंथि को रक्त की अच्छी आपूर्ति होती है । स्वस्थ अवटु ग्रंथि (थायराइड) का अर्थ है—शरीर के परिसंचरण, श्वसन तथा सभी तंत्रों का सही ढंग से कार्य करना ।
यह आसन अवटु ग्रंथि (थायराइड) की आधुनिक चिकित्सा का अच्छा स्थानापन्न है यह आसन कुष्ठ रोग को दूर करता है। उपचार की अवधि में रोगी को मात्र दूध पर निर्भर रहना होता है। दूध अवटु ग्रंथि को पर्याप्त मात्रा में इसका रस स्रवित करने में सहायता करता है, जिससे कि प्रकृति को अपने जीर्णोद्धार एवं पुनर्जीवन के कार्यों में सहायता मिल सके। यदि रोगी प्रातः - सायं सूर्य स्नान करे तो वह शीघ्र स्वस्थ होता है।
यह आसन वृद्धावस्था को नष्ट करता है तथा मनुष्य को सदा युवा रखता है। यह स्वप्न दोष को प्रभावकारी ढंग से रोकता है। यह अजीर्ण, कब्ज, एपेंडिसाइटिस एवं अन्य आमाशय सम्बन्धी रोगों तथा वेरिकोज वेन्स को दूर करता है। यह नाड़ियों की जड़ों को अधिक मात्रा में रक्त की आपूर्ति करता है। यह आसन रक्त को मेरुदंड में केंद्रित करता है तथा इसका पोषण करता है।
इस आसन में मेरुमूल पर्याप्त मात्रा में रक्त खींचते हैं। यह मेरुदंड को लचीला रखता है। रीढ़ का लचीलापन अर्थात चिर यौवन। यह हड्डियों को असमय कड़ा होने से रोकता है। सर्वांग आसन कुंडलिनी को जगाता है तथा जठराग्नि को बढ़ाता है।
यह आसन आपको दृढ़ करेगा तथा आपको नवीन बल और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यह एक आदर्श आसन है। कई लोगों ने मुझे इसके अद्भुत और रहस्यमय लाभदायक परिणामों को बताया है। जब आपके पास अधिक आसन करने का समय न हो तो आप बिना चूके सर्वांग आसन के साथ-साथ शीर्षासन और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। यह आपके डाक्टर के बिल को भी बचायेगा।
समूह २ : शरीर को आगे की ओर मोड़ने वाले आसन
४. पश्चिमोत्तानासन
प्रविधि
भूमि पर कंबल बिछा लें और इसके ऊपर पीठ के बल लेट जायें। धीरे-धीरे उठ कर बैठ जायें। अब श्वाँस को बाहर निकालें और तब तक आगे की ओर झुकें जब तक कि आप दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को न पकड़ लें। धीरे-धीरे आगे की ओर झुकते जायें। आप चित्र में बताये अनुसार अपने चेहरे को घुटनों के मध्य ला सकते हैं। इस आसन में ५ मिनट तक रुकें तथा धीरे-धीरे लेट जायें। अब आप श्वाँस भीतर ले सकते हैं। इसे ३ या ४ बार दोहराएँ ।
जिनको पूर्ण पश्चिमोत्तानासन करने में कठिनाई का अनुभव होता है, वे अर्ध पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। इसके लिए एक पैर दूसरे पैर की जाँघ के पास रखें और दूसरे पैर को सीधा रखें, अब झुक कर इसके पंजे को पकड़ें। अब यही दूसरे पैर से भी करें। कुछ समय बाद रीढ़ लचीली होने पर आप पूर्ण पश्चिमोत्तानासन कर सकेंगे।
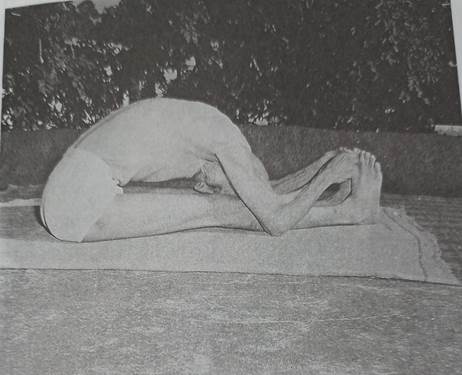
लाभ
यह एक अद्भुत आसन है। यह श्वाँस को ब्रह्मनाड़ी (सुषुम्ना) से प्रवाहित करता है तथा जठराशि बढ़ाता है। इसके अभ्यास से पेट की सभी माँसपेशियाँ प्रभावशाली ढंग से सिकुड़ती है। यह पेट की चर्बी को कम करता है। यह मोटापे तथा तिल्ली एवं यकृत की वृद्धि के निवारण हेतु विशेष लाभप्रद है। यह पेट हेतु शक्तिदायक आसन है। यह आसन पेट के अंगों जैसे वृक्क, यकृत, अग्न्याशय को उत्तेजित करता है। यह आँतों की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है तथा कब्ज को दूर करता है। यह बवासीर को ठीक करता है और मधुमेह को रोकता है। यह आसन नाक्चुरल एमिषन (रात को सोते समय मूत्र की असंयति) हेतु अच्छा प्रतिरोधक है। यह शरीर के पश्च भाग की माँसपेशियों को पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है। इसके अभ्यास से अधिजठरीय नाड़ियाँ, आमाशय, कटि की नाड़ियाँ तथा संवेदी तंत्र अच्छी स्थिति में रहते हैं ।इसके अभ्यास से से रीढ लचीली होती है । जिससे कि स्थायी यौवन स्थापित होता है । हलासन तथा पश्मिोत्तानासन रीढ़ को आगे की ओर सही ढंग से मोड़ते है ।
५. हलासन
जब यह आसन प्रदर्शित किया जाता है, तो हल की भाँति दिखाई देता है ।
प्रविधि
दरी के ऊपर पीठ के बल लेट जायें, हथेलियों को भूमि की ओर रखते हुए दोनों हाथों को जाँघों के पास रखें। पैरों को मोड़े बिना, धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठायें। हाथों को भूमि पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखे रहें । जाँघों तथा कमर का भाग ऊपर की ओर उठायें और पंजों को तब तक नीचे लायें, जब तक कि पंजे सिर के पीछे भूमि को स्पर्श न कर लें। घुटनों को बिलकुल सीधे और पास-पास रखें ।
इस आसन का एक और प्रकार है। जब पंजे भूमि को स्पर्श करें, तो हाथों से पंजे पकड़ लें। यह भी एक अच्छा प्रकार है, अथवा आप अगले उदाहरण में बताए अनुसार भी हाथ रख सकते हैं। इसे ३ या ४ बार कर सकते हैं। आध्यात्मिक लाभ हेतु आपको इस आसन में लम्बे समय तक रुकना चाहिए ।
लाभ
हालांकि भुजंग, शलभ और धनुर आसन में गहरी और सतही माँसपेशियाँ पूरी तरह खिंचती हैं और शिथिल होती हैं, लेकिन हलासन में पीठ की जो माँसपेशियाँ पूरी तरह खिंचती और शिथिल होती हैं, वे रीढ़ को स्वस्थ रखने के लिए उत्तरदायी हैं।
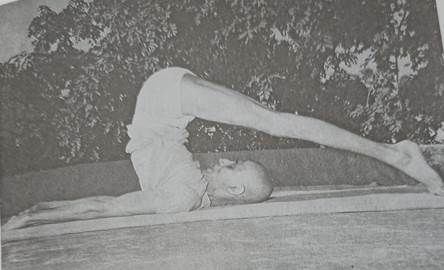
इसके अभ्यास से पेट की माँसपेशियाँ शक्तिशाली रूप से संकुचित होती हैं और दृढ़ बन जाती हैं। इस आसन में संपूर्ण मेरुदंड पीछे की ओर खींचा जाता है, जिससे कि इससे जुड़ी प्रत्येक कशेरुका एवं अस्थि बंधन को प्रचुर मात्रा में रक्त मिलता है और वह दृढ़ हो जाता है। इसके अभ्यास से रक्त की अत्यधिक आपूर्ति होती है और सभी ३१ जोड़ी मेरुनाड़ियों एवं संवेदी तंत्र को पोषण मिलता है तथा उनकी अच्छी मालिश होती है। यह आसन रीढ़ की हड्डी के शीघ्र अस्थिकरण को रोकता है और इसके अभ्यास से मेरुदंड इतना लचीला हो जाता है कि इसको एक कैनवास के टुकड़े की तरह मोड़ा और लपेटा जा सकता है। वह जो इस आसन का अभ्यास करता है। वह अत्यंत फुर्तीला, दीर्घायु तथा ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। यह आसन मेरु नाड़ियों, संवेदी नाड़ी तंत्र, पीठ की माँसपेशियों और कशेरुकाओं की हड्डियों का पोषण करता है । अनेक प्रकार के पेशीशूल, कटिशूल, गले का दर्द तथा स्नायुशूल इसके अभ्यास ये ठीक हो जाते हैं। मोटापा, कब्ज, गुल्म तथा यकृत और प्लीहा के सभी रोग इससे दूर हो जाते हैं ।
६. पादहस्तासन
इसे खड़ा पश्चिमोत्तानासन भी कह सकते हैं। संस्कृत में पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ ।
प्रविधि
सीधे खड़े हो जायें। अपने दोनों हाथ ऊपर करें और पूरी तरह श्वाँस भीतर लें। फिर धीरे-धीरे श्वाँस को बाहर निकालें। इस समय शरीर को तब तक नीचे झुकायें जब तक कि हाथ पंजों तक पहुँच जायें और नासिका घुटनों को स्पर्श करने लगे। घुटनों को दृढ़ और सीधे रखें। पैरों को न मुड़ने दें। ऊपर उठे हुए हाथों को सारे समय यहाँ तक कि शरीर को झुकाते समय भी कानों से स्पर्श करना चाहिए। आप पंजों को पकड़े भी रह सकते हैं। धीरे-धीरे अभ्यास से आप अपने दोनों हाथों को भूमि पर दृढ़ता से जमाए रख कर सिर को दोनों घुटनों से स्पर्श कर सकेंगे। इस आसन में ५ सेकेंड तक रुकें, इसके बाद धीरे से अपने शरीर को उठायें और खड़े हो जायें ।
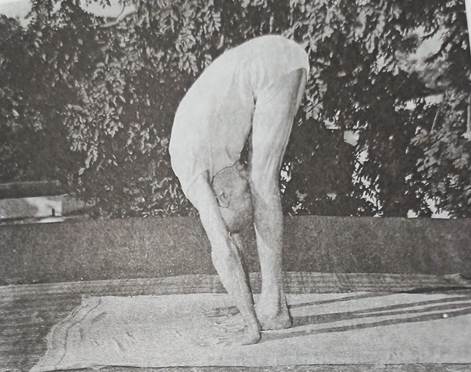
जब आप आप अपने शरीर को उठायें तब आप धीरे-धीरे श्वाँस ले सकते हैं। इसकी ४ बार पुनरावृत्ति करें। कंधों की माँसपेशियों के कड़े होने और पेट के मोटे होने के कारण आप अधिक देर तक पंजों को पकड़े न रह सकते हों, तो घुटनों को थोड़ा सा झुका लें। पंजों को पकड़ लेने के बाद पैरों को सीधे और कड़े कर लें।
लाभ
इस आसन से पश्चिमोत्तानासन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अभ्यास से रीढ़ लचीली और लंबी होती है। आपकी लंबाई बढ़ाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ आसन है। इसके अभ्यास से पेट के ऊपर की चर्बी अदृश्य हो जाती है और शरीर हलका हो जाता है। मोटापा कम करने तथा सुंदर शरीर बनाये रखने के लिए यह आसन स्त्रियों के लिए अत्यधिक अनुकूल है। आपको इस आसन को करने के बाद बहुत अधिक शक्ति का अनुभव होगा। क्योंकि इसके अभ्यास से तमोगुण का निवारण होता है और इस कारण शरीर हल्का हो जाता है।
समूह ३ : शरीर को पीछे की ओर मोड़ने वाले आसन
७. मत्स्यासन
संस्कृत में 'मत्स्य' का अर्थ है, मछली। इस आसन में व्यक्ति जल के ऊपर मछली की भाँति तैरता रह सकता है।

प्रविधि
भूमि पर कंबल बिछा लें और पैर फैला कर बैठ जायें। सीधे पाँव को मोड़ें और एड़ी को बाँयीं जाँघ के जोड़ के ऊपर रख दें। फिर बाँयें पैर को मोड़ें और इसे दाँय जाँघ के जोड़ के ऊपर रख दें। यह पद्मासन है।
इसके बाद पीठ के बल लेट जायें। पद्मासन को भूमि से न उठने दें। कोहनियों अथवा हाथों को भूमि पर टिकायें। अब धड़ और सिर को उठायें। और पीठ को अच्छी तरह झुका कर सिर के शीर्ष भाग को भूमि पर टिकायें। तत्पश्चात् हाथ से पंजों को पकड़ें। यह मत्स्यासन है। इसे सर्वांगासन के तुरंत बाद करना चाहिए। इस आसन में २ या ३ मिनट तक अथवा जितनी देर आप सर्वांगासन करें उससे आधी देर तक रुकें। इसके बाद हाथों की सहायता से सिर को धीरे-धीरे सीधा कर लें। धीरे से बैठ जायें और पद्मासन खोल दें।
जो लोग मोटे होने के कारण पद्मासन नहीं कर सकते, वे मात्र घुटनों से पैरों को मोड़ कर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको गर्दन मोड़ने में तथा सिर का शीर्ष भाग भूमि पर लगाने में तकलीफ हो तो आप अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जा सकते हैं। हाथों को कोहनियों के पास रखें और सिर को हाथों के ऊपर रखें। इस आसन में आप जल पर तैर सकते हैं।
लाभ
यह आसन देर तक सर्वांग आसन करने से उत्पन्न ग्रीवा क्षेत्र की ऐंठन तथा कड़ेपन को दूर करता है। मत्स्यासन गर्दन तथा कंधों की मालिश करता है। सर्वांगासन गर्दन को आगे की ओर अच्छी तरह मोड़ता है, जब कि मत्स्यासन में गर्दन पीछे की ओर मुड़ती है। यह सर्वांग आसन का पूरक आसन है। मत्स्यासन में भी अवटु ग्रंथि तथा परा अवटु ग्रंथि को रक्त की अच्छी आपूर्ति होती है। इससे कमर, पीठ तथा गर्दन शक्तिशाली होती हैं। चूँकि इस आसन में स्वर यंत्र तथा श्वाँस नली अच्छी तरह खुल जाती है, इसलिए अभ्यासी खुल कर तथा गहरी श्वाँस ले सकता है। फेफड़ों का ऊपरी भाग जो कि हँसली के ठीक पीछे स्थित है उसे उचित मात्रा में ताजी हवा और प्राण वायु की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है। गर्दन तथा पृष्ठ क्षेत्र की नाड़ियों को रक्त की अच्छी आपूर्ति होने से उनका पोषण होता है तथा उनकी सही ढंग से मालिश होती है। इसके अभ्यास से अंतःस्रावी ग्रन्थियाँ, मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि एवं पीनियल ग्रंथि उत्तेजित होती हैं तथा उनकी मालिश भी होती है। ये ग्रंथियाँ शरीर के क्रिया विज्ञान सम्बन्धी कार्यों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस आसन में उदर की माँसपेशियाँ खिंचती हैं, इस कारण यह आसन कब्ज दूर करता है तथा पेट के सभी अंगों की मालिश करता है ।
८. भुजंग आसन
जब यह आसन पूर्ण रूप में किया जाता है तो यह फन फैलाये नाग की भाँति दिखाई देता है। इसीलिए इसका नाम भुजंग आसन है।
प्रविधि
कंबल के ऊपर पेट के बल लेट जायें। सभी माँसपेशियों को पूरी तरह ढीली छोड़ दें। दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे रखें। सिर तथा शरीर के ऊपरी भाग को धीरे-धीरे ऊपर उठाये जिस प्रकार नाग अपना फन उठाता है। मेरुदंड को अच्छी तरह मोड़ें। शरीर को अचानक झटके से न उठायें। इसे थोड़ा-थोड़ा उठायें जिससे कि आप वास्तव में एक-एक कशेरुका को मोड़ सकेंगे और दबाव धीरे-धीरे नीचे की ओर जायेगा। नाभि से ले कर नीचे पंजों तक का भाग भूमि से स्पर्श करता रहेगा। आसन में १५ मिनट तक रुकें। फिर सिर को धीरे-धीरे नीचे ले कर आयें। आप इसे ६ बार दोहरा सकते हैं।
सभी पश्चिमी लोगों ने सर्वसम्मति से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन के महत्व को स्वीकार किया है। रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन का अर्थ है— व्यक्ति का स्वास्थ्य, जीवनी शक्ति और यौवन । इससे पीठ की गहरी और सतही माँसपेशियों की अच्छी मालिश होती है। यह आसन अत्यधिक श्रम के कारण उत्पन्न दर्द को दूर करता है। इसके अभ्यास से पेट की माँसपेशियाँ खिचती हैं जिससे वे शक्तिशाली हो जाती हैं। पेट का भीतरी दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है और कब्ज दूर हो जाता है। इसके अभ्यास से पेट के सभी अंगों की अच्छी मालिश होती है।
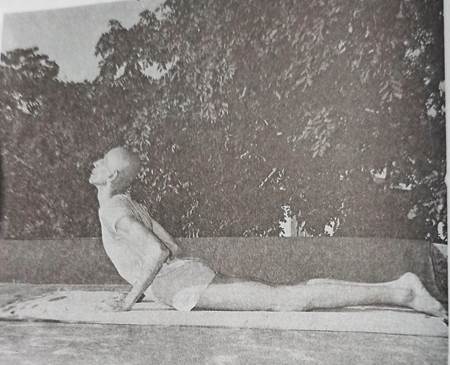
इसके अभ्यास से प्रत्येक कशेरुका तथा इसके अस्थि बंधन पीछे की ओर खिंचते हैं और उन्हें रक्त की पूर्ण आपूर्ति होती है। यह शरीर की गर्मी बढ़ाता है तथा रोगों को नष्ट करता है। इससे भूख भी अच्छी लगती है। स्त्रियों के अंडाशय तथा गर्भाशय की मालिश के लिये यह विशेष रूप से उपयोगी है। यह एक शक्तिशाली शक्ति वर्धक है। यह अनावर्त, कष्टावर्त, प्रदर रोग तथा अन्य गर्भाशय तथा डिम्बग्रंथि सम्बंधी रोगों को दूर करता है।
९. धनुरासन
जब यह आसन किया जाता है तो यह धनुष जैसा दिखाई देता है। 'धनुर' अर्थात धनुष । खिंचे हुए हाथ और पैर धनुष की कमान को अभिव्यक्त करते हैं और शरीर तथा जाँघें धनुष को अभिव्यक्त करते हैं।
प्रविधि
कंबल के ऊपर पेट के बल लेट जायें। माँसपेशियों को ढीला छोड़ दें। घुटनों को मोड़ कर पैरों को जाँघों के ऊपर मोड़ें। सिर और सीने को उठायें। दाँयें टखने को दाँयें हाथ से तथा बाँये टखने को बाँयें हाथ से दृढ़ता से पकड़े। हाथों और पैरों को खींच कर सिर, शरीर तथा घुटनों को उठायें जिससे कि शरीर का संपूर्ण भार पेट पर आ जाये। इसको करने पर रीढ़ धनुष के आकार में मुड़ जाती है। हाथों और कोहनियों को सीधी और दृढ़ रखें और पैरों को अच्छी तरह खींचें जिससे आप सीने को उठा सकें। घुटनों को पास-पास रखें। कुछ देर इसी स्थिति में रहें, तत्पश्चात् शरीर को ढीला छोड़ दें। आप कुंभक करें अथवा सामान्य रूप से श्वाँस लें। यहाँ तक कि दुबले व्यक्ति भी इस आसन को सुंदर ढंग से कर सकते हैं ।
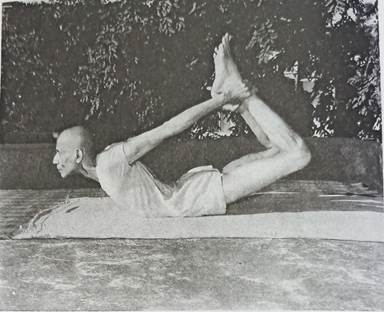
आसन को झटके से न करें। धनुरासन भुजंगासन का पूरक आसन है। जब हम टखनों को पकड़ लेते हैं तो हम इसे भुजंग और शलभ आसन का संयोजन भी कह सकते हैं। भुजंग, शलभ और धनुरासन एक लाभदायक संयोजन है। ये सदा एक साथ किये जाते हैं। ये आसनों का एक समूह निर्मित करते हैं। धनुरासन को ३, ४ बार दोहराया जा सकता है।
लाभ
इस आसन को देखने से लगता है कि यह भुजंग और शलभ आसन का संयुक्त रूप है । शलभ और भुजंग आसन के सभी लाभ धनुरासन में बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसके अभ्यास से पीठ की माँसपेशियों की अच्छी मालिश होती है। यह कब्ज, अजीर्ण, गठिया तथा पेट के सभी रोगों को दूर करता है। यह मोटापा कम करता है। यह पाचन शक्ति एवं भूख में वृद्धि करता है और उदरीय अंगों में रक्त के जमाव को रोकता है। यह आसन स्त्रियों के लिये अत्यंत अनुकूल है। इससे हाथों और पैरों का पूर्ण व्यायाम होता है।
१०. चक्रासन
जब यह आसन किया जाता है तो यह चक्र जैसा दिखाई देता है, इसी कारण इसका नाम चक्रासन है। वास्तव में यह चक्र के स्थान पर धनुष जैसा अधिक दिखाई देता है, अंतर मात्र इतना है कि धनुरासन में शरीर का सम्पूर्ण भार पेट पर रहता है, जब कि चक्रासन में शरीर को हाथों और पैरों का सहारा रहता है । अनेक कलाबाज इसका सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। किशोर बालक इसे बड़ी सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ बहुत लचीली होती है। जब प्रौढ़ावस्था में हड्डियाँ कड़ी हो जाती हैं और उनका अस्थिकरण होने लग जाता है, तो रीढ़ की हड्डी को मोड़ना कठिन होता है, इस कारण उनको इसे करने में कठिनाई होती है।
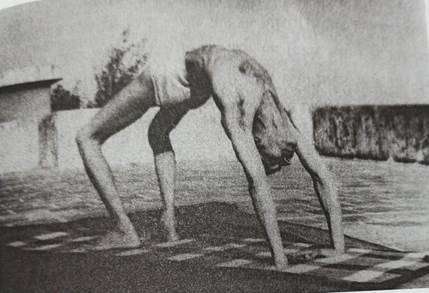
प्रविधि
भूमि पर मोटा कंबल बिछा लें और इस पर खड़े हो जायें। हाथों को ऊपर उठायें, धीरे-धीरे रीढ़ को मोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें। जब आपके हाथ जंघाओं तक पहुँच जायें तो थोड़ा घुटनों को झुकायें, इससे आपको और आगे झुकने में सहायता मिलेगी। अब अपनी हथेलियों को भूमि पर जमा दें। हथेलियों का मुख भूमि की ओर हो। जल्दी न करें, झुकते समय शरीर का पूर्ण संतुलन बनाये रखें, झटके से नीचे न आयें। जब हथेलियाँ भूमि तक पहुँच जायें तो इनको यथासंभव धीरे-धीरे पैरों के पास लाने का बयत्न करें। दुबले व्यक्ति जिनकी रीढ़ लचीली है, वे सरलता पूर्वक टखनों को भी पकड़ लेते हैं। इस आसन में २, ३ मिनट तक रहें और धीरे-धीरे रीर को उठाते हुए खड़े हो जायें। यह चक्रासन है।
यदि आप इस आसन को ऊपर बताए अनुसार नहीं कर सकते हैं, तो इसे दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। दीवार से ३ फीट दूर खड़े हो यें। अपने हाथों को उठायें और हथेलियों को दीवार की ओर रखें। उंगलियाँ भूमि की ओर होनी चाहिए। हाथों को भूमि की ओर धीरे-धीरे ले कर जायें। जब हथेलियाँ भूमि तक पहुँच जायेंगी तो धड़ एक चक्र का आकार बनाएगा। यदि यह विधि भी आपको अनुकूल न हो तो आप अपने मित्र से कह सकते हैं कि वह आपकी जंघाओं को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहे। अब हाथों को ऊपर उठाइये और धड़ का चाप बनाइये। जब हथेलियाँ भूमि तक पहुँच जायें तो अपने मित्र से अपने हाथ छोड़ने के लिए कह दें।
जिनकी रीढ़ कड़ी है अथवा जिनकी पीठ पर चर्बी है, उपरोक्त में से कोई भी विधि उनके लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिये निम्न विधि अनुकूल आएगी। भूमि पर लेट जायें। हाथों को मोड़ कर कंधों के पास रख लें। अब घुटनों को मोड़ कर एड़ियों के पास रखें । शरीर को धीरे-धीरे ऊपर उठायें। इस विधि में धड़ बड़ा ही सुंदर आकार बनाता है। संतुलन बनाते हुए, हाथों को एड़ियों के पास ले कर आयें। आसन पूरा होने पर २ मिनट तक रुकें। हाथों को जमाये रहें तथा पैरों को धीरे-धीरे एक-एक करके पास में लायें। इसके बाद हाथों को एक-एक करके भीतर की ओर खिसकायें ।
एक अन्य विधि है जिसके द्वारा इस आसन के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सीधे लेट जायें, हाथों को कंधों के पास भूमि पर रखें। अब धीरे-धीरे सिर, धड़ और जाँघों को ऊपर उठायें। कोहनियों को सीधी और दृढ़ रखें। दो मिनट तक आसन में रुकें, फिर वापस भूमि पर आ जायें। यदि आप इस आसन को २ या ३ बार दोहरायेंगे तो और भी अच्छा होगा।
लाभ
इसके अभ्यासी का उसके शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह थोड़े से समय में अधिक कार्य कर सकता है। इस आसन से शरीर के सभी अंगों को लाभ पहुँचता है । यदि आप इस आसन को अधिक देर तक नहीं कर सकते हैं तो बार-बार भूमि पर लेट जायें और फिर शरीर उठायें। जब आप आसन करेंगे तो आपका शरीर हल्का हो जायेगा। आपको तत्काल स्फूर्ति का अनुभव होगा। जो लाभ धनुरासन और भुजंगासन से प्राप्त होते हैं, वे सभी आपको चक्रासन के अभ्यास से प्राप्त होते हैं। इसका अभ्यास पादहस्तासन अथवा पश्चिमोत्तानासन के पश्चात् करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। चक्रासन के अभ्यास से हाथ, अग्र भुजाओं, जौधों तथा पैरों को शक्ति प्राप्त होती है।
११. सुप्त वज्रासन
इसे करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन सीखना होगा। यह नमाज अदा करने की स्थिति से मिलता-जुलता है। कंबल बिछा कर घुटनों के बल बैठ जायें, अब इसी स्थिति में नीचे बैठ जायें, इस स्थिति में नितंब तलवों के ऊपर रहेंगे। धड़, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें। हथेलियों को घुटनों पर रखें। घुटने पास-पास रखें। कोहनियों को न मोड़ें। यह वज्रासन है। आप इस आसन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अजीर्ण से पीड़ित लोगों को इससे बहुत अधिक लाभ होता है। भोजन के पश्चात् आप इस आसन में थोड़ी देर अवश्य बैठें। इससे पैरों और हाथों की नाड़ियाँ शक्तिशाली होती हैं तथा घुटनों, पैरों, पंजों एवं जाँघों का पेशीशूल अदृश्य हो जाता है। पेट में गैस बननी बंद हो जाती है। शरीर के सर्वाधिक आवश्यक अंग कंद (जहाँ से ७२००० नाड़ियाँ निकलती हैं) के ऊपर वज्रासन से बड़ा ही लाभदायक प्रभाव पड़ता है। यह आसन पैरों, जंघाओं तथा रीढ़ हेतु अत्यंत उत्तम है।
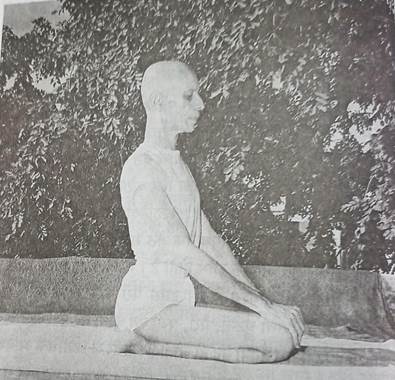
प्रविधि
सुप्त वज्रासन वज्रासन और मत्स्यासन का संयुक्त रूप है। सुप्त वज्रासन में घुटनों पर वज्रासन की तुलना में अधिक जोर पड़ता है। एक कंबल पर वज्रासन में बैठ जायें। पैरों और जाँघों को जमाये रखें। हाथों और कोहनियों के सहारे पीठ के बल लेट जायें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा कर सिर के नीचे रख लें। उंगलियों को फँसाने के स्थान पर, मत्स्यासन की भांति भी आप हथेलियों को रख सकते हैं। आसन में २ से ५ मिनट तक रुकें ।
लाभ
इस आसन में आपको वज्रासन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अभ्यास से कुबड़ापन दूर हो जाता है। यह उदरीय अंगों हेतु अच्छा व्यायाम है। मत्स्यासन तथा धनुरासन के सभी लाभ इस आसन के अभ्यास से प्राप्त होते हैं । इसे पश्चिमोत्तानासन अथवा पादहस्तासन के अभ्यास के पश्चात् करें ।
समूह ४ : बगल की ओर झुकने वाले आसन
१२. त्रिकोणासन
इस आसन को करने पर यह त्रिकोण के समान दिखाई देता है, इस कारण इसे त्रिकोणासन कहते हैं।
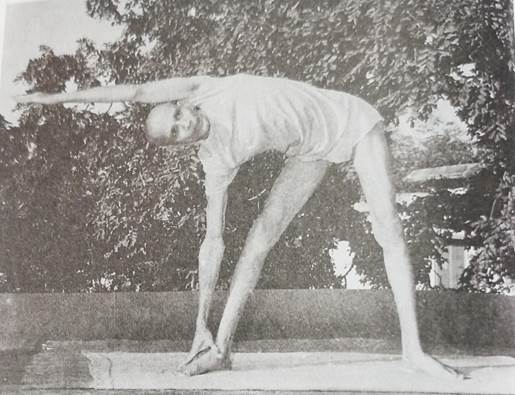
प्रविधि
हथेलियों को भूमि की ओर होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को कमर से बाँयीं ओर धीरे से झुकायें और बाँयें हाथ से बाँयें पंजे को स्पर्श करें। आप सिर को भी थोड़ा झुका सकते हैं। आसन में ५ सेकेंड रुकें और वापस धीरे से खड़े हो जायें । जब आप झुकें अथवा खड़े हों तो हाथों और पैरों को मुड़ने न दें। अब आप दाँयीं ओर मुड़ें और पूर्वानुसार दाँयें हाथ से दाँयें पंजे को स्पर्श करें। ५ सेकेंड रुर्के और पुनः पूर्ववत खड़े होने की स्थिति में आ जायें। यह त्रिकोणासन है। इसे प्रत्येक ओर से ४ बार करें।
लाभ
त्रिकोणासन मेरु नाड़ियों तथा उदरीय अंगों की मालिश करता है. आँतों की क्रमाकुचन गति में वृद्धि करता है और भूख बढ़ाता है। इसके अभ्यास से कब्ज दूर हो जाता है। शरीर हल्का हो जाता है। जिनको कमर, जंघा अथवा पैर में फ्रैक्चर के कारण पैर छोटा होने की शिकायत होती है. उनको इसके अभ्यास से लाभ होता है। इसमें धड़ की माँसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, शिथिल होती हैं और खिंचती हैं, इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। श्रीमान मुलर ने भी अपने शारीरिक व्यायाम की क्रियाओं में इसका विवरण दिया है। एक योगी के लिए मेरुदंड बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह मेरुरज्जु तथा संवेदी तंत्र से संयुक्त है। त्रिकोणासन का अभ्यास मेरुदंड को स्वस्थ रखता है तथा यह मेरुनाड़ियों की अच्छी तरह मालिश करता है।
१३. ताड़ासन
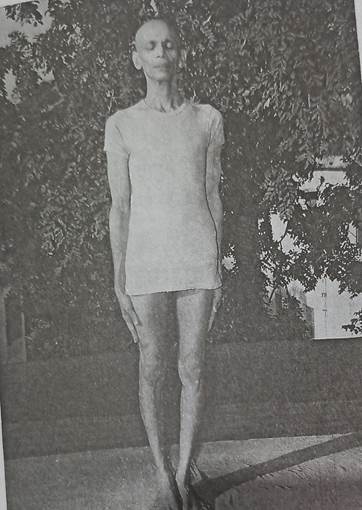
यह विद्यालयों में विद्यार्थियों को सामान्य रूप से कराया जाता है। हाथों को बाजू में रख कर सीधे खड़े हो जायें। अब एक हाथ को सिर के ऊपर शीघ्रता से खींचें। हाथ को मुड़ने न दें, फिर इसे पूर्व स्थिति में ले आयें। यही अब अन्य हाथ से करें। इसे जितनी बार चाहें, उतनी बार दोहरा सकते हैं। यह आसन दोनों हाथों को एक साथ उठा के भी किया जा सकता है, या कि जब हाथ कंधों के समानांतर अथवा भूमि के समानांतर पहुँच जायें, तो आप थोड़ी देर रुर्के फिर हार्थों को ऊपर ले जायें। यही आसन हाथों को सामने की ओर तथा बगल में ले जा कर भी किया जाना चाहिए। यह हार्थो के लिये बहुत अच्छा है । जैसे ही यह आसन समाप्त हो जाये, हाथों और कंधों की माँसपेशियों की मालिश करें।
समूह ५ : मेरुदंड को मोड़ने वाले आसन
१४. अर्ध मत्स्येंद्र आसन
'अर्ध' का अर्थ है आधा। यह मत्स्येंद्र आसन का आधा है। इसका नाम योगी मत्स्येंद्रनाथ के कारण रखा गया है, जिन्होंने सर्वप्रथम इस आसन को हठयोग के अभ्यासियों को सिखाया था ।
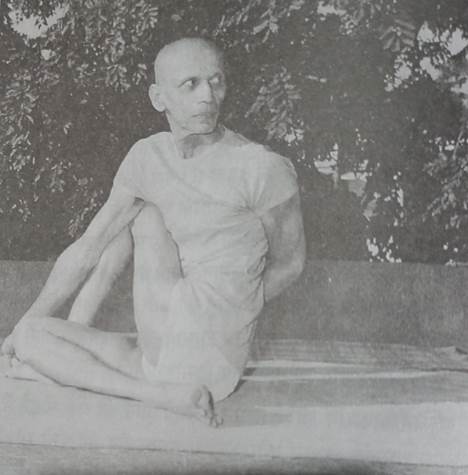
प्रविधि
भूमि पर कंबल बिछा लें और इस पर पैर फैला कर बैठ जायें। दाँयें पैर का घुटने से मोड़ें और एड़ी को मूलाधार में लगायें। एड़ी को इस स्थान से न हिलने दें। बाँयें पैर को घुटने से मोड़ें और हाथों की सहायता से इसे दाँय जाँघ के बाहरी ओर भूमि पर जमायें। इसके बाद सीधे हाथ को बाँयें घुटने से नीचे ले जा कर इससे बाँयें पंजे को दृढ़ता से पकड़ें। बाँयाँ घुटना दाँयीं बगल में लगा होना चाहिए। रीढ़ को और अधिक घुमाने के लिए बाँयें हाथ को पीछे की ओर मोड़ कर दाँयीं जाँघ को पकड़ें। अब धीरे से रीढ़ को घुमायें और बाँयीं ओर मुड़ें। रीढ़ को एक समान घुमाने के लिए गर्दन को भी बाँय ओर घुमायें । सीने को सीधा और आगे की ओर रखें। इसी विधि को पैर बदल कर, रीढ़ को दाँयीं ओर घुमा कर दोहरायें और इस प्रकार दोनों तरफ से रीढ़ को घुमायें। यह रीढ़ को पूर्ण रूप से मोड़ता है।
पश्चिमोत्तानासन और हलासन रीढ़ को आगे की ओर मोड़ते हैं, जब कि धनुरासन, भुजंग आसन और शलभ आसन रीढ़ को पीछे मोड़ते हैं। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसे घुमाना तथा दाँयें-बाँयें भी मोड़ना चाहिए। मात्र तभी रीढ़ पूरी तरह लचीली रह सकेगी। रीढ़ को दाँयें-बाँयें मोड़ने के लिए मत्स्येंद्र आसन बहुत अच्छा है।
अर्ध मत्स्येंद्र आसन रीढ़ को लचीला रखता है तथा उदरीय अंगों की अच्छी मालिश करता है। कटिवात तथा पीठ की पेशियों के सभी प्रकार के
पेशीशूल इसके अभ्यास से दूर हो जाते हैं। इसके अभ्यास से रीढ़ के नाड़ी मूल तथा सवेदी तंत्र की मालिश होती है तथा उनको रक्त की अच्छी आपूर्ति होती है। यह कब्ज तथा अजीर्ण के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस आसन में प्रत्येक कशेरुका दोनों तरफ से घूमती है, कशेरुका से जुड़े अस्थि बंधनों को भी यह गति मिलती है और उनको रक्त की अच्छी आपूर्ति होती है। सभी मेरु नाड़ियों की मालिश होती है। यह आसन बहुत अधिक मात्रा में पार्श्व गति प्रदान करता है ।
समूह ६ : पेट के आसन
१५. शलभ आसन
जब इस आसन का प्रदर्शन किया जाता है, तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि शलभ अपनी पूँछ उठाये हुए हो। इसीलिए इसे शलभ आसन कहते हैं।
प्रविधि
कंबल के ऊपर पेट के बल लेट जायें। हाथों को शरीर के पास रखें। हथेलियाँ ऊपर की ओर रहेंगी। मस्तक को थोड़ा ऊपर उठा कर ठोढ़ी को भूमि पर लगाये रखें। अब श्वाँस भीतर लें। सारे शरीर को कड़ा कर लें और पैरों को भूमि से लगभग हाथ भर ऊपर उठायें। ध्यान रहे, घुटने एकदम सीधे रहें। त्रिकास्थि भी पैरों के साथ थोड़ा ऊपर उठेगी। अब धड़ तथा हाथों को पैरों के भार का अनुभव होगा। जाँघों, पैरों तथा पंजों को एक सीधी रेखा में रखें। इस आसन में २० सेकेंड तक रहें और धीरे-धीरे पैरों को नीचे लायें और धीरे-धीरे श्वाँस छोड़ दें। इस आसन को अपनी क्षमता के अनुसार ३ अथवा ४ बार दोहरायें, लेकिन इतना अधिक न करें कि थकान आ जाये। भुजंगासन शरीर के पिछले भाग का व्यायाम कराता है तथा शलभासन शरीर के निम्न बाह्य अंग का । कुछ व्यक्ति इसमें भुजंगासन की भाँति हथेलियों को सीने के पास रखते हैं।
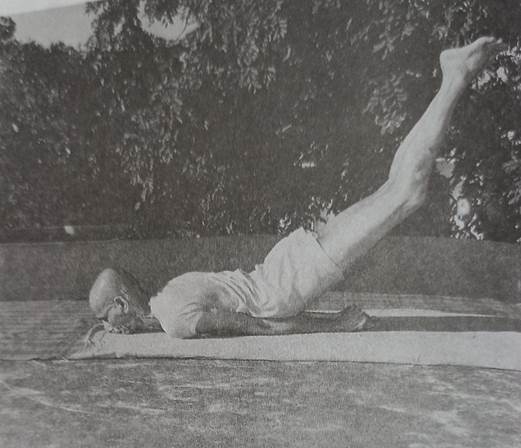
लाभ
इसके अभ्यास से पेट के भीतर का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह कब्ज को दूर करता है तथा इसके अभ्यास से यकृत, अग्न्याशय तथा वृक्क की मालिश होती है और पेट की सभी माँसपेशियाँ अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। कमर तथा त्रिकास्थि की कशेरुकाओं की मालिश होती है। त्रिकज, अनुत्रिक तथा निम्न कटिक्षेत्र को प्रचुर मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है और वे शक्तिशाली बनते हैं। इस आसन को करते समय कुंभक करने से फेफड़े फैलते हैं और बलशाली बनते हैं। यह पेट और आँतों के कई रोगों को दूर करता है। यह यकृत की सूजन को दूर करता है। कटि क्षेत्र के सभी प्रकार के पेशीशूल इससे ठीक हो जाते हैं। यह मेरुदंड के पिछले भाग को मोड़ता है । यह पश्चिमोत्तानासन अथवा पादहस्तासन का पूरक आसन है। भुजंगासन शरीर के ऊपरी आधे भाग का विकास करता है, जब कि शलभासन शरीर के निचले आधे भाग का तथा निचले अंतिम भाग का विकास करता है।
१६. मयूर आसन
संस्कृत में मयूर का अर्थ है 'मोर'। जब यह आसन प्रदर्शित किया जाता है तो यह बिल्कुल मोर की भाँति दिखाई देता है। इस आसन को करने के लिये अच्छी शारीरिक शक्ति आवश्यक है ।
कंबल के ऊपर घुटनों के बल बैठ जायें। दोनों हथेलियों को जोड़ कर भूमि पर रखें। उंगलियाँ पैरों की ओर होनी चाहिए। आप उंगलियों को थोड़ा फैला सकते हैं। इससे आपको संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी। हाथों को दृढ़ता पूर्वक जमाए रखें। इससे आपको संपूर्ण शरीर के सहारे के लिए स्थिर और दृढ़ आधार प्राप्त होगा। पेट को धीरे से जुड़ी हुई कोहनियों के ऊपर रखें। अपने शरीर को कोहनियों पर सहारा दें। अब अपने पैरों को फैलायें और पंजों को भूमि पर टिकायें। श्वाँस भरें और पैरों को एक साथ भूमि से ऊपर उठायें। पैरों को भूमि के समानांतर सिर के बराबर उंचाई तक उठायें। इसी स्थिति में ५ सेकेंड तक रहें, फिर पंजों को भूमि पर रख दें और श्वाँस बाहर छोड़ दें। यह मयूर आसन है। कुछ मिनट तक विश्राम करें। व्यायामी इस आसन को मेज को किनारे से पकड़ कर सकते हैं।
लाभ
यह आसन पेट के रोगों के लिये अतिश्रेष्ठ है। हाथों का दबाव नाभि के नीचे पड़ने के कारण उदर की बड़ी धमनी आंशिक रूप से दबती है और रुका हुआ रक्त पाचन अंगों की ओर जाता है एवं यकृत, अग्न्याशय, आमाशय तथा वृक्क की मालिश होती है। इसके अभ्यास से अंतर उदरीय दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा सभी उदरीय अंगों की मालिश होती है। मयूरासन से हथेलियों की माँसपेशियाँ शक्तिशाली हो जाती हैं। मयूरासन से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है।
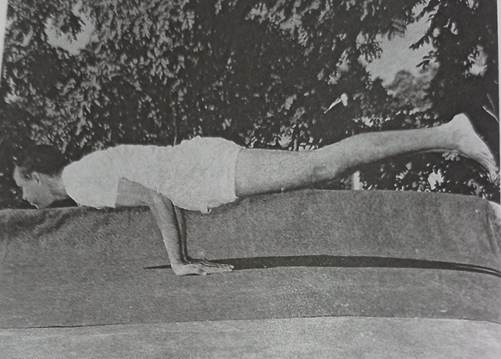
मयूरासन का स्वयं का आकर्षण है। यह आपको शीघ्र शक्ति प्रदान करता है। यह एडरीनेलिन या डायजीनेटिक के हायपोडर्मिक इंजेक्शन का कार्य करता है। यह पाचन हेतु अद्भुत आसन है। यह अजीर्ण तथा पेट के रोगों का उपचार करता है।
इससे यकृत की सूजन अदृश्य हो जाती है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जो नित्य कुछ देर तक करने मात्र से आपको शारीरिक व्यायाम के अधिकतम लाभ प्रदान करता है।
१७. लोलासन
यह झूला झूलने का एक प्रकार है। यह मयूरासन और पद्मासन का संयुक्त रूप है। इसके लिए पहले आपको लंबे समय तक मयूरासन का अभ्यास करना होगा। जब आप मयूरासन सरलता पूर्वक और सुख पूर्वक करने लगें तब आप लोलासन का अभ्यास कर सकते हैं। मयूर आसन में आ जायें, आसन को स्थिर रखें। पैरों को मोड़ कर पद्मासन लगा ले । यह लोलासन है। आप चाहें तो पहले भी पद्मासन लगा सकते हैं और फिर हाथों को मयूरासन की भाँति भूमि पर रखें, घुटने भूमि पर रहेंगे। पेट कोहनियों पर टिकायें, अब धीरे से पैरों को उठायें। यह भी एक अच्छा प्रकार है। मयूरासन के सभी लाभ लोलासन से प्राप्त होते हैं।
समूह ७ : शिथिलीकरण विद्या
वर्तमान काल में जीवन अत्यंत जटिल हो गया है, अस्तित्व के लिये संघर्ष बहुत अधिक बढ़ गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक प्रतियोगिता है। रोटी की समस्या को हल करना बहुत अधिक कठिन हो गया। है । सर्वत्र बेरोजगारी है। बुद्धिमान नवयुवक जिनके पास असाधारण प्रतिभा है तथा सिफारिश है, मात्र उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। इस कारण आधुनिक मनुष्य के ऊपर न समाप्त होने वाले दैनिक कार्यों तथा अस्वास्थ्यकर जीवन पद्धति के कारण निरंतर शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता रहता है।
कार्य गति उत्पन्न करते हैं, गति आदत का कारण होते हैं। मानव ने बहुत सी कृत्रिम आदतें अपना ली हैं। उसने अपनी प्राकृतिक मूल आदतों को भुला दिया है। गलत आदतों के कारण उसने अपनी माँसपेशियों तथा नाड़ियों पर तनाव डाल दिया है।
वह शिथिलीकरण के प्रथम सिद्धान्त को भूल गया है। आज उसे कुत्ते, बिल्ली और शिशु से शिथिलीकरण की विद्या सीखने की आवश्यकता है।
यदि आप शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे तो आप अत्यंत क्रियाशील और ऊर्जावान होंगे। शिथिलीकरण में माँसपेशियाँ और नाड़ियाँ विश्राम की स्थिति में होती हैं और उनमें प्राण या ऊर्जा का संग्रहण और संरक्षण होता है। अधिकांश लोग शिथिलीकरण की इस सुंदर क्रिया को नहीं जानते, वे माँसपेशियों और नाड़ियों पर अनावश्यक दबाव डाल कर, माँसपेशियों में अनावश्यक गति उत्पन्न करके अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। कुछ लोग बैठे-बैठे अनावश्यक रूप से पैरों को हिलाते रहते हैं। कुछ लोग जब उनका मन खाली या बेकार होता है, तो अपनी उंगलियों से कुछ तबला बजाते रहते हैं। कुछ सीटी बजाते हैं, कुछ सिर हिलाते हैं, कुछ अपनी उंगलियों से पेट पर थाप देते हैं। शिथिलीकरण क्रिया के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान न होने के कारण, विभिन्न शारीरिक अंगों की अनावश्यक गतिविधियों द्वारा ऊर्जा का अपव्यय होता रहता है।
आलस्य को शिथिलीकरण समझने की भूल न करें। आलसी मनुष्य अकर्मण्य होता है। उसे काम करने में कोई रुचि नहीं होती है। वह आलस्य और सुस्ती से भरा रहता है। वह नीरस रहता है। वह मनुष्य जो शिथिलीकरण करता है, उसमें शारीरिक बल, ऊर्जा, जीवनी शक्ति और सहन शक्ति होती है। वह थोड़ी मात्रा में भी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देता। वह बहुत ही कम समय में किसी भी कार्य को अद्भुत ढंग से सम्पन्न कर सकता है।
जब आप किसी कार्य को करने के लिये किसी माँसपेशीको संकुचित करना चाहते हैं, तो मस्तिष्क से नाड़ी द्वारा उस माँसपेशी को तरंग भेजी जाती है और ऊर्जा अथवा प्राण को प्रेरक नाड़ी द्वारा भेजा जाता है, फिर यह माँसपेशी तक पहुँचती है और उसके अंतिम छोर को खींचती है। जब माँसपेशी संकुचित होती है तो आप जिस पैर को चलाना चाहते हैं, उसे ऊपर की ओर खींचती है और आप इस क्रिया को सरलता से कर पाते हैं। सर्वप्रथम विचार आता है, फिर यही विचार माँसपेशियों के सकुचन क्रिया का रूप ले लेता है।
कल्पना कीजिए, आप एक कुर्सी को उठाना चाहते हैं। यह इच्छा मन में एक तरंग उत्पन्न करती है। यह तरंग मस्तिष्क से प्रेरक नाड़ियों द्वारा हाथ की कोशिकाओं को भेजी जाती है। मस्तिष्क से नाड़ियों के साथ प्राण ऊर्जा भेजी जाती है, जिससे माँसपेशी सिकुड़ती है और आप कुर्सी उठाने का कार्य कर पाते हैं। इसी प्रकार सभी कार्य चेतनावस्था अथवा अचेतनावस्था में आपके द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। यदि माँसपेशियाँ अधिक श्रम कर लेती हैं, तो अधिक ऊर्जा व्यय होती है और आपको थकान का अनुभव होता है। अधिक श्रम तनाव या खिंचाव के कारण प्राण या ऊर्जा का अधिक व्यय होता है, जिससे माँसपेशियों की अधिक क्षति होती है।
जब आप किसी काम को चेतनावस्था में करते हैं, तो मन को सन्देश भेजा जाता है और मस्तिष्क जरूरतमंद अंग को ऊर्जा भेज कर तत्काल इस आदेश का पालन करता है। अचेतन अवस्था में काम सहज प्रेरणा अथवा यांत्रिक रूप से होता है।
जब कोई बिच्छू आपकी उंगली पर दंश लगाता है तो मन आपके आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता और उंगली तुरंत खींच ली जाती है। यह विवाद का विषय नहीं है, यह सहज और यांत्रिक प्रक्रिया है। शीघ्र उत्तेजित होने वाला मनुष्य मन की शांति का उपभोग नहीं कर सकता । उसका मस्तिष्क, नाड़ियाँ और माँस-पेशियाँ सदा तनाव में रहती हैं। वह अत्यधिक मात्रा में पेशी ऊर्जा, नाड़ी ऊर्जा एवं मानसिक शक्ति का अपव्यय करता है। ऐसा मनुष्य यदि शक्ति सम्पन्न हो तो भी वह अत्यंत कमजोर मनुष्य है, क्योंकि वह अत्यंत सरलता से अपना संतुलन खो देता है। यदि आप वास्तव में शांति और स्थाई सुख का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको चिंता, आकुलता, भय, क्रोध के आवेग तथा अन्य लोगों को दबाने वाली प्रवृत्ति को दूर कर अपने मन को शांत, नियंत्रित और संतुलित रखना होगा।
आप अनावश्यक रूप से चिंता करके, अकारण क्रोध करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्रोध पाशविक वृत्ति से जुड़ा हुआ है। क्रोध, मस्तिष्क, रक्त और नाड़ियों को प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचाता है। आपको क्रोध के प्रदर्शन से किंचित भी लाभ नहीं होगा। किसी भी क्रिया को बार-बार करने से मन में एक आदत बन जाती है। यदि आप बार-बार चिंता करेंगे तो चिंता करने की आदत बन जायेगी। चिंता, क्रोध तथा भय के द्वारा आपकी जीवनी शक्ति और ऊर्जा सरलता से बह जाती है।
आप किसी भी बात से डरते क्यों हैं ? सभी आपकी अपनी आत्मा हैं। भय, क्रोध और चिंता अज्ञानता की उपज हैं। क्रोध और चिंता के शिकार व्यक्ति की माँसपेशियाँ और नाड़ियाँ सदा संकुचित और तनाव में रहती हैं।
एक समूह की माँसपेशियों की क्रिया विधि दूसरे समूह की माँसपेशियों द्वारा रोकी जा सकती है। यदि कोई तरंग एक समूह की माँसपेशियों को तुरंत गति में लाने का प्रयास करती है, तो आप दूसरे समूह की माँसपेशियों द्वारा प्रतिरोधक आवेग भेज कर प्रथम समूह की माँसपेशियों की क्रिया विधि को रोक सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है तो आप तत्क्षण ही उसे मारने दौड़ पड़ते हैं। एक समूह की माँसपेशियों को बिना विचारे ही एकदम से काम करने का आदेश मिल जाता है। किंतु आप विवेक और 'मैं उसे मार कर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकूँगा। वह अज्ञानी है। वह यह भी नहीं जानता कि व्यवहार कैसे करना चाहिए? मुझे उसे क्षमा कर देना चाहिये' ऐसी विपरीत भावना द्वारा उस आवेग को रोक सकते हैं। यह आवेग तत्काल ही द्वितीय समूह की माँसपेशियों द्वारा प्रथम समूह की माँसपेशियों को काम करने से रोक देगा। आवेगों, साथी आवेगों तथा प्रतिरोधी आवेगों में वृद्धि। नाडियों, माँसपेशियों और मस्तिष्क में भारी तनाव होता है। बहुत से व्यक्त आवेगों के दास होते हैं, इसलिये वे मन की शांति का उपभोग नहीं कर पा वे इधर-उधर भटकते रहते हैं।
शिथिलीकरण की क्रियाविधि एक सटीक विद्या है। इसे अत्यंत सरलता पूर्वक सीखा जा सकता है। माँसपेशियों के संकुचन की ही भांति माँसपेशियों का शिथिलीकरण भी महत्वपूर्ण है । मैं मन, नाड़ियों तथा माँसपेशियों के शिथिलीकरण पर बहुत अधिक बल देता हूँ। शिथिलीक के लिये शवासन निर्दिष्ट है।
१८. शवासन
'शव' का अर्थ है मृत शरीर । जब कोई इस आसन को करता है तो वह मृत शरीर के समान दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम शवासन है। यह आसन सबसे अंत में किया जाता है।
प्रविधि
एक नर्म कंबल बिछायें तथा उस पर पीठ के बल लेट जायें। हाथों को बगल में रखें। पैरों को सीधे रखें। एड़ियों को पास-पास रखें और पंजों को दूर-दूर । आँखें बंद कर लें। अब शरीर की सभी माँसपेशियों को ढीला छोड़ दें। श्वाँस धीरे-धीरे और एक लय में लें। उमड़ते हुए विचारों को शांत कर लें और अपने विचारों को भीतर निर्दिष्ट करें। सभी माँसपेशियों, नाडियों और अंगों को ढीला छोड़ दें।
शिथिलीकरण क्रिया का प्रारंभ पंजों से करें, तत्पश्चात् तलवों, पिंडलियों, जाँघों, गर्दन, चेहरे आदि की पेशियों को शिथिल करते जायें। ध्यान रखें कि उदरीय अंगों, हृदय, सीना, मस्तिष्क आदि भी शिथिल होना चाहिए। स्वयं को आदेश दें-"सोना नहीं है।" इस आसन में आपको पूर्ण शांति, आराम तथा शिथिलीकरण का अनुभव होगा। आपको इस आसन के लाभदायक परिणामों का अनुभव होगा। इसे सभी आसनों के अंत में करना चाहिये ।
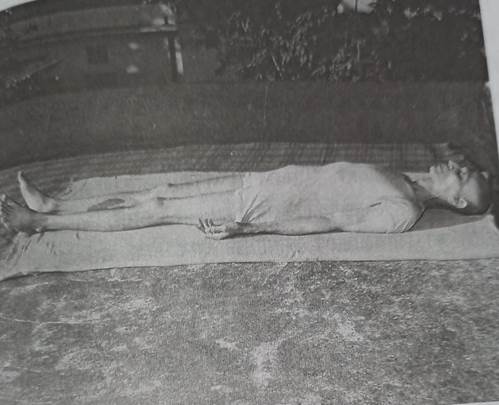
लाभ
जो इस आसन को सफलता पूर्वक कर सकते हैं उनको ही आसनों के सुखदायक और आनंददायक अनुभव प्राप्त होते हैं। इस अनुभव का शब्दों में ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। आप में से प्रत्येक को इसका आनंद लेना चाहिये। यदि आप कठिन परिश्रम से थक गये हैं, तो इस आसन को ५ मिनट के लिए कीजिए, आप पुनः पूर्ववत शक्ति से पूर्ण हो जायेंगे। यह सभी कठोर परिश्रमी लोगों के लिये वरदान है।
यदि आप चाहें तो आसनों और व्यायाम के पश्चात् आराम कुर्सी पर लेट कर भी शिथिलीकरण कर सकते हैं। जो शिथिलीकरण जानते हैं, वे जब चाहें थोड़ी देर के लिए झपकी ले सकते हैं। व्यस्त लोगों, चिकित्सकों और वकीलों को शिथिलीकरण क्रिया का ज्ञान होना चाहिये, वे रेलवे प्रतीक्षालयों, अदालत के कमरों, क्लीनिक आदि स्थानों में भी मन को शिथिल करके विश्राम कर सकते हैं। इस प्रकार वे अपने अगले काम के लिए पुनः तैयार हो सकते हैं। शिथिलीकरण मनुष्य को पूर्ण विश्रान्त कर देता है।
विद्यार्थी, पत्रकार, व्यस्त वकीलों, चिकित्सकों और व्यवसायी जनों को मानसिक शिथिलीकरण का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए । जो इस आंतरिक और बाह्य शिथिलीकरण की क्रियाविधि का ज्ञान नहीं रखते वे अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का बहुत ह्रास करते हैं। जो इस क्रिया का अभ्यास करते हैं, वे अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करके इसका प्रयोग अपने अधिकतम लाभ हेतु कर सकते हैं। योगियों को इस क्रिया का भली-भाँति ज्ञान होता है। वे इस विद्या के स्वामी होते हैं। जो शिथिलीकरण का अभ्यास करते हैं उन्हें कभी भी थकान का अनुभव नहीं होता। वे खड़े-खड़े ही कुछ देर तक आँखें बंद करके स्वयं को अगले कार्य हेतु तैयार कर लेते हैं। जिस प्रकार नल खोलने से जल प्रवाहित होता है उसी प्रकार शिथिलीकरण करने से नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाहित होती है।
माँसपेशियों के व्यायाम में शिथिलीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। हल, सर्वांग, पश्चिमोत्तान, धनुर एवं अर्धमत्स्येंद्र आसन में शरीर की सभी माँसपेशियाँ बहुत अधिक खिंचती और संकुचित होती हैं। पेशियों की अत्यधिक क्रियाशीलता से चयापचय बढ़ जाता है (उपचय और अपचय परिवर्तन जो शरीर में होते हैं उन्हें चयापचय कहते हैं) माँसपेशियाँ जो अत्यधिक तनाव में रहती हैं, उन्हें शिथिलीकरण तथा विश्राम की आवश्यकता रहती है। यह शवासन ही है, जो शीघ्र तथा प्रभावकारी ढंग से पूर्ण विश्राम तथा आराम प्रदान करता है।
समूह ८ : ध्यान के आसन
आसनों को दो बड़े समूहों में बाँटा जा सकता है—ध्यान के आसन और स्वास्थ्य तथा शक्ति के आसन । योग शास्त्र के अनुसार ध्यान हेतु चार श्रेष्ठ आसन हैं—पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन एवं सुखासन ।
आपको इन चारों में से किसी एक आसन में शरीर को बिना हिलाये एक साथ तीन घंटे तक बैठने का अभ्यास होना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जितना अधिक आप आसन में स्थिर होंगे उतना अधिक आप धारणा करने तथा मन को एकाग्र करने योग्य होंगे।
उपरोक्त चारों में से जो भी आपको अनुकूल हो उस आसन को चुन लें तथा १५ मिनट बैठें और धीरे-धीरे इस अवधि को तीन घंटे तक बढ़ायें । जब आप आसन में बैठें तो सिर, गर्दन और धड़ को सीधा रखें। पीठ को झुकायें नहीं। जब आप ध्यान के लिये आसन में बैठें तो अपनी आँखे बंद कर लें और त्रिकुटि, नासिका के अग्र भाग अथवा अनाहत चक्र पर धारणा करें।
१९. पद्मासन
यह महत्वपूर्ण आसनों में से एक है। जब पद्मासन प्रदर्शित किया जाता है तो यह कमल के समान दिखाई देता है। संस्कृत में 'पद्म' का अर्थ है कमल । इस आसन में दोनों पैर विपरीत जंघाओं पर रखे हुए कमल की पंखुड़ियों को अभिव्यक्त करते हैं। इसे कमलासन भी कहते हैं।
ध्यान के चारों आसनों पद्म, सिद्ध, स्वस्तिक और सुखासन में से पद्मासन प्रथम स्थान पर आता है । यह ध्यान हेतु सर्वश्रेष्ठ आसन है। घेरण्ड, शांडिल्य तथा अन्य ऋषियों ने इस आसन की बहुत प्रशंसा की है। यह गृहस्थों, पुरुषों तथा स्त्रियों सभी के लिये अनुकूल है ।
प्रविधि
उपरोक्त में से कोई भी एक आसन जप और ध्यान हेतु प्रयोग किया जा सकता है।
ध्यान के कमरे में अपने इष्ट देवता अथवा गुरु के चित्र के सामने एक कुशासन बिछा लें और इसके ऊपर मृगचर्म अथवा बाघ की छाल का आसन बिछा लें, फिर ध्यान के लिए बैठ जायें। आप एक सूती कपड़े का टुकड़ा बिछा कर उसके ऊपर मृगचर्म अथवा बाघ की छाल का आसन बिछा लें, तत्पश्चात् ध्यान के लिए बैठ जायें अथवा भूमि पर चारवर्ती कंबल बिछा लें और इस पर एक कपड़ा बिछा लें, यह भी ठीक होगा।
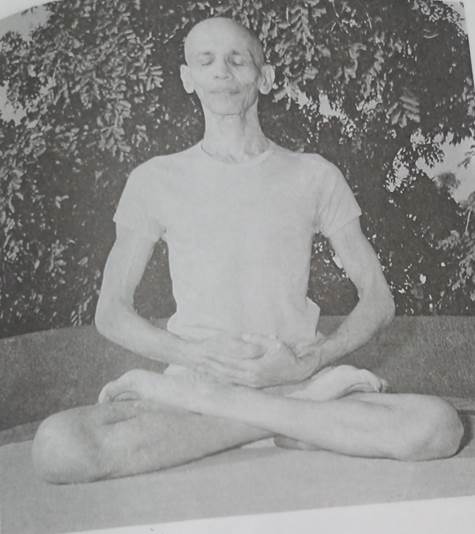
इस आसन पर बैठें और पैरों को सामने फैलायें। दाँयें पंजे को दोनों हाथों से पकड़ें और पैर को घुटने से मोड़ कर पंजे को बाँय जाँघ पर रखें। इसी प्रकार बाँयें पैर को मोड़ें और दाँयीं जंघा पर रखें। शरीर को सीधा रखें। हाथों को एक के ऊपर एक रख कर (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) एड़ियों के बीच रखें। यदि यह आपको अनुकूल नहीं आ रहा है तो आप अन्य उदाहरण एक के अनुसार रख सकते हैं। ध्यान रहे, बाँया घुटना अथवा जाँघ को भूमि से ऊपर नहीं उठना चाहिए।
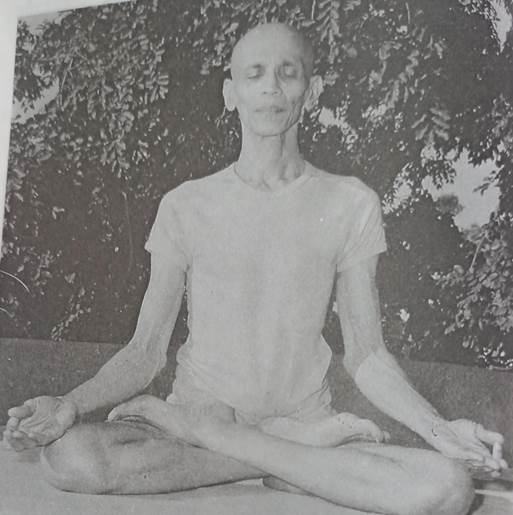
लाभ
ये ध्यान के आसन जप तथा ध्यान हेतु अत्यधिक अनुकूल हैं। ये जठराग्नि में वृद्धि करते हैं तथा अच्छी भूख, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करते हैं। ये गठिया रोग दूर करते हैं। ये वायु, कफ और पित्त को संतुलित रखते हैं । ये पैरों और जाँघों की नाड़ियों को शुद्ध करते हैं और उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। ये ब्रह्मचर्य पालन हेतु लाभदायक हैं।
२०. उत्थित पद्मासन
इसका अभ्यास स्वास्थ्य के उद्देश्य से किया जाता है। पद्मासन में बैठ जायें। हाथों को भूमि पर बाजू में रखें और पद्मासन लगाये हुए शरीर को उठायें। कुछ सेकेंड तक रुकें और नीचे भूमि पर आ जायें। यह हाथों की माँसपेशियों के लिए अच्छा आसन है।
२१. सिद्धासन
चूँकि अनेक सिद्धजन ध्यान हेतु इस आसन का प्रयोग करते रहे हैं, इस कारण इसका नाम सिद्धासन है। सिद्ध योगियों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है । पद्मासन के बाद सिद्धासन महत्वपूर्ण है। युवा ब्रह्मचारी तथा जो ब्रह्मचर्य में स्थापित होना चाहते हैं उन्हें इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कई लोग इसे पद्मासन की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं।
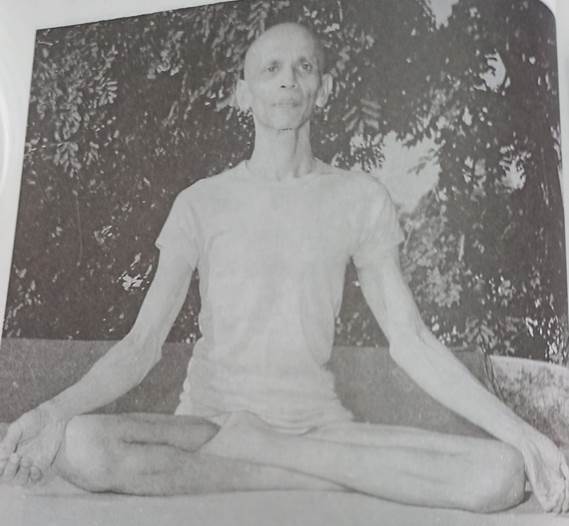
प्रविधि
अपने आसन पर बैठ जायें। पैरों को सामने की ओर फैला लें। बाँयें पैर को घुटने से मोड़ लें और एड़ी को गुदा और अंडकोष के बीच के स्थान पर रखें। फिर दाँयें पैर को मोड़ें और एड़ी को पुरोनितम्बीय अस्थि अथवा जननांग के ठीक ऊपर रखें। शरीर को सीधा रखें तथा हाथों को पद्मासन की भाँति रखें।
सिद्धासन को वीरासन, मुक्तासन और गुप्तासन भी कहते हैं। घेरण्ड संहिता में इन आसनों को पैरों की थोड़ी भिन्न स्थिति के साथ वर्णित किया गया है।
२२. स्वस्तिक आसन
संस्कृत में स्वस्तिक का अर्थ है समृद्धि । यह आसन अभ्यासी को समृद्धि, सफलता तथा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, इसलिए यह स्वस्तिक आसन कहलाता है।
प्रविधि
आसन पर बैठ जायें। अपने पैर सामने की ओर फैला लें। दाँयें पैर को घुटने से मोड़ लें और एड़ी को बाँय जाँघ के सामने रखें, जिससे कि तलवा जाँघ की माँसपेशियों के एकदम पास रहे।
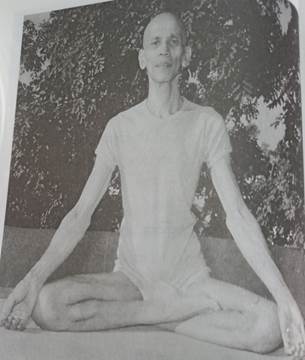
इसी प्रकार बाँयें पैर को मोड़ें और इसे दाँयीं उरुसंधि (पेट और जाँघ के बीच का दबा हुआ भाग) के सामने रखें। बाँयें पैर के तलवे को दाँयीं पिंडली और जाँघ की माँसपेशियों के बीच फंसायें। अब आपके दोनों पैर पिंडलियों तथा जाँघ की माँसपेशियों के बीच में होंगे। एकदम सीधे बैठे। यह आसन ध्यान हेतु उत्तम है। हाथों को उसी प्रकार रखे जैसा पद्मासन में निर्दिष्ट किया गया है।
२३. सुखासन
स्वस्तिक आसन को सुखासन भी कहते हैं। प्राणायाम, जप तथा ध्यान हेतु जिस आसन में सुखपूर्वक बैठा जा सकता है, उसे सुख आसन कहा जाता है। किसी भी सरल आसन में जिसमें आप सिर, गर्दन तथा धड़ को सीधा रख कर बिना हिले-डुले लंबे समय तक आराम से बैठ सकते हैं, उसे सुखासन कहते हैं।
आप ध्यान के चारों आसनों में से कोई भी एक आसन चुन सकते हैं। जब आप आसन में बैठें तो इंद्रियों पर संयम रखें और दोनों भौंहों के मध्य त्रिकुटि पर धारणा करें ।
आसनों हेतु निर्देश
१. हठयोग प्रदीपिका और अन्य पुस्तकों में आपको अनेक आसन मिलेंगे । इस पुस्तक में मैंने कुछ चुने
हुए महत्वपूर्ण आसनों के बारे में लिखा है, जो पूर्व तथा पश्चिम के लोगों के अनुकूल हैं।
२. आसनों के समूह इस प्रकार बनाये गये हैं कि इनमें से प्रत्येक समूह में से नित्य एक या दो आसनों का
अभ्यास करने से अभ्यासी के शरीर का पूर्ण विकास होता है।
३. अपने स्वभाव, क्षमता तथा उपलब्ध समय के अनुसार आपको एक या दो आसनों का चुनाव करना है;
लेकिन आपको प्रत्येक समूह में से एक आसन अवश्य लेना है। इससे आपके शरीर का पूर्ण विकास होगा।
४. समूह २ के सभी आसनों में आप आगे की ओर झुकते हैं। इन आसनों में आपकी माँसपेशियाँ संकुचित
होती हैं। इनसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये आपको तुरंत ही कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करना होगा। जिनमें माँसपेशियाँ खिंचती हैं, उदाहरण के लिये यदि आप पश्चिमोत्तानासन, हल आसन अथवा पादहस्तासन का अभ्यास करते हैं तो आपको तुरंत ही मत्स्यासन, भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन अथवा सुमवज्रासन का अभ्यास करना चाहिये। अतः शरीर के सर्वांगीण विकास के. लिए आपको आगे झुकना, पीछे झुकना, दाँयें-बाँयें झुकना, रीढ़ को घुमाना आदि आसनों का अभ्यास करना होगा। सभी आसनों के अंत में शवासन का अभ्यास करना चाहिए, तभी अभ्यास पूर्ण होता है।
५. समूह ७ में ध्यान के लिए चार आसनों का वर्णन किया गया है। आप किसी भी ऐसे आसन का चुनाव
कर सकते हैं जिसमें आप लंबे समय तक आराम से बैठ सकें। ये आसन प्राणायाम, जप तथा ध्यान के अभ्यास लिए अनुकूल हैं। भक्त स्वाध्याय करते समय भी उसी आसन में बैठ सकते है, जिसमें ध्यान करते हैं।
६. प्रारंभ में १५ मिनट के लिए आसन में बैठें और इस अवधि को धीरे-धीरे तीन घंटे तक बढ़ायें और ऐसा
होने पर आपको आसन सिद्धि अथवा आसन जय प्राप्त होगी। फिर आप एक चित्त मन से अपने ध्यान में आगे बढ़ सकेंगे। बिना स्थिर आसन के आप ध्यान में अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जितना अधिक आप अपने आसन में स्थिर होंगे, उतना ही अधिक आप धारणा कर सकेंगे।
७. कुछ देर बाद यदि पैरों में बहुत अधिक दर्द होने लगे तो आसन को खोल दें, तत्पश्चात् ५ मिनट तक
पैरों की मालिश करें, तत्पश्चात् पुनः आसन में बैठ जायें। जब आप नित्य अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। कभी पद्मासन, कभी सिद्धासन इस प्रकार बार-बार आसन को न बदले। एक आसन में दृढ़ रहे ।
८. हठयोग की पुस्तकों में पद्मासन और सिद्धासन के लाभों के बारे में बहुत अधिक वर्णन मिलता है। ये
आसन जठराग्नि में वृद्धि करते हैं और अच्छी भूख, उत्तम स्वास्थ्य तथा आनद प्रदान करते हैं। ये गठिया दूर करते हैं और वात, पित्त और कफ को संतुलित रखते हैं। ये पैरों और जाँघों की नाड़ियों को शुद्ध करते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं।
९. प्रातःकाल ४ बजे उठ जायें। शौच हेतु जायें। मुँह धो लें। इसके | बाद आसन, प्राणायाम और ध्यान का
अभ्यास करें। यदि आप ध्यान हेतु अधिक समय देते हों, तो आधा घटे आसन और प्राणायाम करें, तत्पश्चात् ध्यान हेतु बैठें। ध्यान के पश्चात् आधे घंटे विश्राम करें अथवा थोड़ी देर घूमने चले जायें। बाद में आप शेष आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंधों का अभ्यास कर सकते हैं।
१०. यदि आपको प्रातः शीघ्र शौच के लिये जाने की आदत नहीं है, तो आप शौच के लिये जाये बिना ही
आसनों का अभ्यास कर सकते हैं । लेकिन योग साधकों को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें शौच के पश्चात् ही सभी आसनों का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए रात के समय तथा प्रातःकाल बिस्तर से उठने के तत्काल बाद शीघ्र ठंढा अथवा गर्म जल पियें और अपने आहार को नियमित एवं समायोजित करें।
११. आसनों के अभ्यास के समय एक लंगोटी अथवा कौपीन धारण करें। आप बनियान भी पहन सकते हैं।
आसन करते समय चश्मा न पहनें। यह टूट सकता है और आँखों में चोट लग सकती है।
१२. अपने अभ्यास में नियमित रहें। जो लहर में आ कर अभ्यास प्रारंभ करते हैं, उन्हें अधिक लाभ प्राप्त
नहीं होता। यदि कोई आसनों तथा प्राणायाम से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभ्यास में नियमितता बहुत अधिक आवश्यक है। सामान्यतया लोग प्रारंभ में एक या दो बड़ी रुचि पूर्वक तथा उत्साह के साथ अभ्यास करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। यह एक बड़ी भूल है। आसनों और प्राणायामों का लंबे समय तक नियमित अभ्यास कीजिए और आश्चर्यजनक लाभों का साक्षात्कार कीजिए। माह तक
१३. शारीरिक व्यायाम प्राणों को बाहर ले जाते हैं, जब कि आसन प्राणों को अंदर भेजते हैं। आसन प्राणों को
सारे शरीर में तथा विभिन्न तंत्रों में समान रूप से वितरित करते हैं। आसन मात्र शारीरिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होते हैं, क्योंकि वे कुंडलिनी शक्ति का जागरण करते हैं। विशेष आसन किसी विशेष रोग को दूर करते हैं। आसन रोग प्रतिरोधक भी हैं। आसन इंद्रियों, मन तथा शरीर के नियंत्रण में बहुत सहायता करते हैं। इनसे शरीर, नाड़ियाँ एवं माँसपेशियाँ शुद्ध होती हैं।
१४. प्रारंभ में आप कुछ आसनों को पूर्ण रूप से नहीं कर सकेंगे। नियमित अभ्यास से इनमें पूर्णता आएगी।
इस हेतु धैर्य, लगनशीलता तथा उत्साह आवश्यक है।
१५. आसनों के बीच हल्का कुंभक करने से आसन की सामर्थ्य में वृद्धि होती है तथा यह अभ्यासी के बल
और जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। आसन के साथ-साथ जप और प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। तभी यह सच्चा योग बनेगा। जो मंत्र जप करते हैं, वे आसन के साथ-साथ भी इसे जप सकते हैं। व्यस्त लोग जिनके पास अत्यंत कम समय होता है, वे भी आसन के साथ-साथ जप कर सकते हैं। यह उसी तरह है जैसे कि एक पत्थर फेंकने से चार फलों को प्राप्त करना। आपको इससे कई सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी।
१६. जो शीर्षासन तथा अन्य आसनों का अभ्यास लंबे समय तक करते हैं, उन्हें अभ्यास की समाप्ति पर
हल्का नाश्ता अथवा एक प्याला दूध लेना चाहिए।
१७. संपूर्ण अभ्यास में आपको सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको एक प्रकार का भोजन
अनुकूल नहीं आ रहा है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन लायें। यदि कोई विशेष आसन आपको अनुकूल नहीं आ रहा है तो अधिक परिश्रम न करें और उसी समूह में से कोई अन्य आसन चुन ले, यह युक्ति है। अभ्यास करते समय आपमें स्फूर्ति होना चाहिए। यदि आप कोई विशेष आसन नहीं कर पा रहे है तो दुःखी न हों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बार-बार प्रयत्न करे। निरतर अभ्यास तथा बार-बार प्रयत्न करने से आपको सफलता मिलेगी।
१८. कोई भी आदत जो शरीर को दुर्बल करती हो, वह विभिन्न रोगों को लाने में सहायक होती है। कोई भी
चीज जो जीवनी शक्ति को घटाती हो, वह शरीर की गंदगी दूर करने की सामर्थ्य को कम करती है। अल्कोहल युक्त पेय, तम्बाकू, कोकेन, अफीम, गाँजा, भाँग, दुराचरण तथा किसी भी प्रकार की अति को पूर्णतया त्याग दें।
१९. आसनों का अभ्यास प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद आसन
नहीं करना चाहिए; क्योंकि इस समय शारीरिक ऊर्जा का उपयोग पाचन में होता है। आसनों का अभ्यास खुले हवादार कमरे, खुले बरामदे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे अथवा बगीचे में किया जा सकता है।
२०. जब आप योगासनों का अभ्यास करें तो सात्विक भोजन लेना आवश्यक है। दूध, घी, बादाम, फल,
मलाई आदि लें। प्याज, लहसुन, माँस, मछली, धूम्रपान, शराब, खट्टे तथा तीखे भोज्य पदार्थ त्याग दें। पेट को अधिक न भरें।
२१. योगासन करने के तत्काल बाद कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं किया जाना चाहिए; क्योंकि सभी
आसन आंतरिक ऊतकों तथा अगो को शक्ति प्रदान करने के लिए किये जाते हैं और इसी के अनुसार उन्हें रक्त की आपूर्ति की जाती है। लेकिन शारीरिक व्यायाम माँसपेशियों को स्वस्थ करते। हैं, इस कारण शारीरिक व्यायाम करते समय रक्त माँसपेशियों की ओर खिंचता है और रक्त के संचरण की दिशा विपरीत हो जाती है और योगाभ्यासी को आसनों का लाभ नहीं प्राप्त होता है। अतः आसन करने के पश्चात् कुछ देर विश्राम करें, तत्पश्चात् शारीरिक व्यायाम आरंभ करें।
२२. एक वेदांती आसन और प्राणायाम करने से डरता है, क्योंकि वह सोचता है कि इनका अभ्यास उसका
देहाध्यास तीव्र करेगा तथा यह उसके वैराग्य के विपरीत होगा। हालाँकि हठयोग और वेदांत दो भिन्न मार्ग हैं, फिर भी वेदांती आसनों और प्राणायामों को संयुक्त करके अधिक लाभ ले सकते हैं। मैंने कई वेदांतियों को दुर्बल तथा रोगी शरीर वाला देखा है। शरीर का मन के साथ अत्यंत निकट सम्बंध है। दुर्बल तथा रोगी शरीर का अर्थ है— दुर्बल तथा रोगी मन । यह शरीर आपके लिए लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक घोड़े के समान है। हालाँकि शरीर जड़ और निरुपयोगी है; लेकिन यह आत्म साक्षात्कार हेतु महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे स्वच्छ, बलशाली तथा स्वस्थ रखा जाना चाहिए। यदि वेदांती थोड़ा योगाभ्यास करें तो यह उनके शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली रखने हेतु पर्याप्त होगा। वे अच्छी साधना कर सकेंगे और शीघ्र लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे।
२३. हिंदू धर्म में प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राण का मन के साथ सम्बंध है और मन के
द्वारा यह इच्छा के साथ सम्बंधित है, इच्छा के द्वारा यह व्यक्ति की आत्मा से और इसके द्वारा यह परमात्मा से सम्बद्ध है। यदि आपको मन के द्वारा प्राण की छोटी-छोटी लहरों को कैसे नियंत्रित किया जाये इसका ज्ञान है, तो विश्व प्राण पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जाये इसका ज्ञान हो जायेगा। श्वसन क्रिया पर नियंत्रण के द्वारा आप शरीर में प्रवाहित हो रही संपूर्ण नाड़ी ऊर्जा को सफलता पूर्वक नियंत्रित कर सकेंगे। जिसने प्राण के इस सार पर नियंत्रण कर लिया है, उसने मात्र शरीर पर ही विजय नहीं पाई वरन् विश्व के प्रत्येक शरीर और प्राण पर विजय प्राप्त कर ली है। प्राणायाम वह साधन है जिसके द्वारा योगी विश्व की सम्पूर्ण शक्ति को प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।
२४. जिसका मन शांत है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसकी गुरु तथा शास्त्रों के वचनों में
श्रद्धा है तथा जो आहार और शयन में संयमित है तथा इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलने हेतु उत्सुक है, ऐसा व्यक्ति योगाभ्यास हेतु योग्य है। ऐसा व्यक्ति प्राणायाम के अभ्यास में सफलता प्राप्त कर सकता है।
२५. वृक्षासन : यह विभिन्न प्रकार से किया जाता है। शीर्षासन को वृक्षासन कहा जाता है। उंगलियों को
आपस में फंसाने के स्थान पर यदि आप कंधों के पास दोनों हथेलियों को रख कर शीर्षासन में खड़े हो जायें तो इसे वृक्षासन भी कहते हैं। आपने कई व्यायामियों को इस प्रकार खड़े देखा होगा । वृक्षासन का एक अन्य प्रकार निम्नानुसार है— सीधे खड़े रहें। एक पैर को घुटने से मोड़ें और इसे दूसरे घुटने पर रखें। हाथों को अपने सीने के पास रखें। आसन में स्थिर रहें। यह भी वृक्षासन है। पहले बाँयें पैर पर खड़े हों, फिर दाहिने पैर पर ।
२६. पर्वत आसन : पद्मासन में बैठ जायें। धीरे से हाथों और शरीर को ऊपर उठायें। मात्र घुटने भूमि पर
रहेंगे। आप उंगलियों को आपस में फंसा कर भी रख सकते हैं। यदि आप घुटनों पर नहीं खड़े रह सकते तो आप भूमि पर बैठ कर हाथों को ऊपर कर सकते हैं। यह भी अच्छा है। पद्मासन में बैठने के स्थान पर आप वज्रासन में बैठ कर फिर शरीर और हाथ को ऊपर उठायें। इस प्रकार में शरीर को घुटनों तथा पंजों पर टिका रहेगा।
२७. एक ही आसन के विभिन्न नाम होते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन को उग्रासन भी कहते हैं। पद्मासन का
कमलासन भी कहते हैं। सिद्धासन को वीरासन, मुक्तासन और गुप्तासन के नाम से जाना जाता है। शवासन को मृतासन भी कहते हैं।
अध्याय २
प्राणायाम
प्राणायाम क्या है ?
प्राण सर्वव्यापक ऊर्जा का मूल है। यह जीवनी शक्ति है। यह सर्वव्यापक है। यह स्थिर या गत्यात्मक अवस्था में हो सकती है। यह उच्च से लेकर निम्न तक, चींटी से ले कर हाथी तक, एक कोशीय अमीबा से ले कर मनुष्य तक, पौधों के आरम्भिक जीवन से ले कर पशुओं के विकसित जीवन तक सभी रूपों में पाया जाता है। यह प्राण ही है जो आपके नेत्रों में चमकता है। यह प्राण की ही शक्ति है, जिससे कि कान सुनते हैं, आँखें देखती हैं, त्वचा अनुभव करती है, नासिका सूंघती है, मस्तिष्क और बुद्धि अपना कार्य करते हैं।
युवा तरुणी की मुस्कुराहट, संगीत में मिठास, एक वक्ता के प्रभावशाली शब्द, किसी प्रिय व्यक्ति की बातों का आकर्षण — ये सभी प्राण के कारण हैं। अग्नि प्राण से प्रज्वलित होती है। वायु प्राण के द्वारा बहती है। नदियाँ प्राण से बहती हैं। भाप का इंजिन प्राण के द्वारा कार्य करता है। रेल और कार प्राण के द्वारा चलती हैं। रेडियो की तरंगें प्राण के द्वारा प्रवाहित होती हैं। प्राण इलेक्ट्रान है। प्राण बल है। प्राण चुम्बकत्व है। प्राण विद्युत है। यह प्राण ही है जो हृदय से रक्त को धमनियों में भेजता है। यह प्राण है जो पाचन, उत्सर्जन और निष्कासन करता है।
चिंतन, संकल्प, कार्य करने, चलने, लिखने आदि के द्वारा प्राण का विस्तार होता है। एक स्वस्थ, बलवान मनुष्य में प्रचुर मात्रा में प्राण अथवा नाड़ी बल अथवा जीवनी शक्ति होती है। भोजन, जल, वायु, सौर ऊर्जा आदि के द्वारा प्राण की आपूर्ति होती है। प्राण को नाड़ी तंत्र द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। प्राण का अवशोषण श्वास द्वारा होता है। अतिरिक्त प्राण मस्तिष्क तथा नाड़ी केंद्रों में संग्रहित रहता है। जब वीर्य ऊर्जा का शोधन अथवा रूपांतरण होता है, तो यह शरीर को प्रचुर मात्रा में प्राण की आपूर्ति करता है और यह प्राण ओज़ के रूप में मस्तिष्क में संग्रहित रहता है। ओज और कुछ नहीं, वरन् प्राण ही है।
योगी प्राणायाम के नित्य अभ्यास द्वारा प्रचुर मात्रा में प्राण का संग्रहण करता है । वह योगी जिसने अत्यधिक मात्रा में प्राण का संग्रहण किया है, वह अपने चारों ओर शक्ति और जीवनी शक्ति का विकिरण करता है। वह एक बड़ा शक्ति का केंद्र है। यह वैसे ही है जैसे कि बैटरी में विद्युत संग्रहित रहती है। जो योगी के साथ निकट संपर्क में आते हैं, वे उससे प्राण को अवशोषित करते हैं और शक्ति, बल, जीवनी शक्ति तथा आत्मा का आनंद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार जल एक बर्तन से दूसरे बर्तन की ओर प्रवाहित होता है, प्राण वास्तव में एक स्थिर तरंग की भाँति एक विकसित योगी से दुर्बल व्यक्तियों की ओर प्रवाहित होता है। वह योगी जिसने आंतरिक दृष्टि का विकास कर लिया हो वह इसे प्रत्यक्ष देख सकता है ।
प्राण तथा शरीर की विभिन्न जीवनी शक्तियों के नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं। यह श्वाँस का नियमन है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है। प्राणायाम का लक्ष्य है—प्राण पर नियंत्रण। इसका प्रारंभ श्वाँस के नियमन के साथ जीवन तरंगों के पूर्ण नियंत्रण के द्वारा होता है। अन्य शब्दों में प्राणायाम श्वाँस के नियंत्रण द्वारा जीवन तरंगों पर पूर्ण नियंत्रण है । प्राणायाम के नियमित अभ्यास द्वारा सही श्वसन की आदत स्थापित की जानी चाहिये। सामान्यतया लोगों में श्वसन क्रिया अनियमित होती है।
यदि आप प्राण पर नियंत्रण कर सकते हैं तो आप विश्व के मानसिक तथा शारीरिक समस्त बलों पर नियंत्रण कर सकते हैं। योगी उस प्रगट सर्वव्यापक शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है, जिससे सभी शक्तियाँ (चुम्बकत्व, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण, संयोग, नाड़ी तरंगों, जीवनी शक्ति अथवा विचार शक्ति से सम्बन्धित शक्तियाँ, वास्तव में विश्व की सभी शक्तियाँ) उत्पन्न होती हैं ।
यदि कोई श्वाँस अथवा प्राण पर नियंत्रण कर सकता है तो मन भी स्वयं ही नियंत्रित हो जाएगा। वह जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, उसने अपनी श्वाँस पर भी नियंत्रण पा लिया है। यदि इनमें से कोई एक अधीन हो जायेगा तो दूसरा भी अधीन हो जायेगा। यदि मन तथा शरीर दोनों ही नियंत्रित हो जायें तो व्यक्ति इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जायेगा और अमरता को प्राप्त करेगा। मन, प्राण और वीर्य में अंतरंग सम्बंध है, यदि कोई वीर्य पर नियंत्रण प्राप्त कर ले तो मन और प्राण भी नियंत्रित हो जायेंगे। जिसने वीर्य शक्ति को नियंत्रित कर लिया है, उसने अपने प्राण और मन पर भी नियंत्रण कर लिया है।
यदि आप कोई अत्यंत धीमी ध्वनि को सुनना चाहते हैं, तो कुछ देर के लिए आपकी श्वाँस रुक जायेगी। जो कुली रेलवे स्टेशन पर चावल के भारी बोरे ले जाता है, वह पहले अपने फेफड़ों को वायु से भरता है और इस प्रकार जब तक वह थैले को अपनी पीठ पर रखता है, तो वह अनजाने ही प्राणायाम का अभ्यास करता है । इस प्रकार के अन्य उदाहरण हैं जैसे :- वह जो कूद कर छोटा नाला पार करता है, जो लम्बी कूद या ऊंची कूद का अभ्यास करता है तथा जो पैरेलल बार पर विभिन्न प्रकार के व्यायामों का अभ्यास करता है, ये सभी सहज रूप से वायु को भीतर रोकने (कुंभक) का अभ्यास करते हैं। यह कुंभक उसकी जीवनी शक्ति तथा बल में वृद्धि करता है। यह उसे तत्काल प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। जिस प्रकार सुनार भट्ठी को फुंकनी के द्वारा जलाता है, फिर सोने को इस गर्म भट्ठी में पिघला कर इसकी अशुद्धियों को दूर करता है, उसी प्रकार योगाभ्यासी प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर तथा इंद्रियों की अशुद्धियों को दूर करता है।
प्राणायाम का मुख्य लक्ष्य है प्राण और अपान को एक करना और इस संयुक्त प्राण तथा अपान को धीर-धीरे सिर की ओर ऊपर ले कर जाना। प्राणायाम का प्रभाव अथवा परिणाम है, सोती हुई कुंडलिनी का जागरण।
प्रथम महत्वपूर्ण चरण है आसनों पर स्वामित्व अथवा शरीर पर नियंत्रण । अगली क्रिया है प्राणायाम । प्राणायाम के सफल अभ्यास हेतु सही आसन अनिवार्य पूर्वापेक्षा है । कोई भी सरल आरामदेह स्थिति आसन कहलाती है। वह आसन श्रेष्ठ है, जिसमें कि अधिकतम समय तक आराम से बैठा जा सके। आसन करते समय धड़, गर्दन और सिर एक सीध में होने चाहिए। आपको शरीर को आगे-पीछे अथवा दाँयें-बाँयें झुकाना नहीं है। आपको झुक कर नहीं बैठना है। नियमित अभ्यास से आसन में स्वयं ही दक्षता आती हैं। मोटे होने के कारण जो पद्मासन में बैठने में कष्ट का अनुभव करते हैं, वे सुखासन अथवा सिद्धासन में बैठ सकते हैं। आपको प्राणायाम हेतु आसन में पूर्ण दक्षता आने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आसनों का अभ्यास करें और साथ-साथ प्राणायाम का भी अभ्यास करते रहें। कुछ समय बाद आपको दोनों में दक्षता प्राप्त हो जायेगी। प्राणायाम का अभ्यास कुर्सी पर सीधे बैठ कर भी किया जा सकता है।
भगवद्गीता में आपको आसन और बैठने की स्थिति के बारे में सुंदर विवरण प्राप्त होता है। एक शुद्ध एकांत स्थान में स्वयं के एक निश्चित आसन में बैठें जो न अधिक ऊँचा हो न अधिक नीचा। सबसे पहले एक कुशासन बिछायें, उसके ऊपर एक मृग की छाल, इस पर एक कपड़ा बिछा लें। अब इस पर मन को एकाग्र करके तथा विचारों और इंद्रियों को संयमित करके स्थिर बैठ कर आत्म शुद्धि के लिए उसे योगाभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा तथा दृढ़ रख कर दृष्टि को नासिकाग्र पर केंद्रित करना चाहिए (गीता : ६/१०, ११ और १२ ) ।
प्राणायाम चूँकि श्वाँस से सम्बद्ध है, इसलिये इसके द्वारा विभिन्न आंतरिक अंग तथा संपूर्ण शरीर का अच्छा व्यायाम होता है। प्राणायाम सभी रोगों को दूर करता है, स्वास्थ्य का विकास करता है, पाचन को ऊर्जा प्रदान करता है, नाड़ियों को शक्ति प्रदान करता है, वासनाओं को दूर करता है और कुंडलिनी शक्ति का जागरण करता है। यह अच्छा स्वास्थ्य और स्थिर मन प्रदान करता है । प्राणायाम का अभ्यासी अपनी श्वाँस को रोक सकता है। प्राणायाम के कई अभ्यासी अपने सीने पर पत्थर भी तोड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण पर नियंत्रण कर लिया है। प्राणायाम के अभ्यासी का शरीर हल्का और रोगों से मुक्त होता है। उसकी वाणी मधुर होती है। उसके शरीर से मीठी सुगंध आती है।
जो प्राणायाम का अभ्यास करता है उसको अच्छी भूख लगती है। वह प्रसन्न रहता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। वह बलवान, साहसी, उत्साही एवं स्वस्थ होता है। उसके मन की धारणा अच्छी होती है। प्राणायाम पूर्व तथा पश्चिम के सभी स्त्री-पुरुषों के लिए अत्यधिक अनुकूल है।
एक योगी अपने जीवन की लंबाई वर्षों की संख्या से नहीं, वरन् श्वाँसों की संख्या से मापता है। आप प्रत्येक श्वाँस के साथ वायुमंडलीय वायु से ऊर्जा अथवा प्राण की एक विशेष मात्रा भीतर लेते हैं। कोई मनुष्य अधिकतम श्वाँस की जितनी मात्रा यथा संभव भीतर ले सकता है, वह क्षमता जीवन क्षमता कहलाती है। एक मनुष्य एक मिनट में १५ बार श्वाँस लेता है। प्रतिदिन श्वाँसों की संख्या है २१,६०० ।
जिस कमरे में आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वह सीलन भरा और बंद नहीं होना चाहिए, यह सूखा और हवादार होना चाहिए। आप नदी या झील के किनारे, बगीचे के कोने में अथवा खुली हवा में प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अधिक ठंढी हवा नहीं होनी चाहिए और यह स्थान पहाड़ी की चोटी पर नहीं होना चाहिए। मन को सत्य पर दृढ़ रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास नित्य करने से चित्त सुषुम्ना में लीन होता है और फिर यह विचलित नहीं होता और फलस्वरूप प्राण स्थिर हो जाता है। प्राणायाम हेतु गहन धारणा एवं एकाग्रता आवश्यक है।
प्राणायाम में किसी भी अवस्था में तनाव नहीं होना चाहिए। आपको प्राणायाम करते समय आनंद का अनुभव होना चाहिए। सदैव पूरक और रेचक अत्यंत धीरे-धीरे करें। किंचित भी आवाज न होने दें। जब भी आप असहज और हताशा का अनुभव करें, प्राणायाम का अभ्यास करें।
प्राणायाम में कुंभक का अभ्यास करने से गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे कि कुंडलिनी शक्ति जाग्रत होती है और यह सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर जाती है। कुंभक जीवन काल में भी वृद्धि करता है। आसन के समय कुंभक करने से आसन की सामर्थ्य में वृद्धि होती है और यह अधिक बल और जीवन शक्ति प्रदान करता है। प्राणायाम के अभ्यास के समय अपने इष्ट मंत्र का जप करते रहिये। यही सच्चा योग होगा।
यदि आपको बिस्तर से जागने के पश्चात् सदा ही आलस्य रहता है, तो आप नींद को भगाने तथा ध्यान हेतु १० प्राणायाम कुंभक सहित करें। मन प्राणायाम के अभ्यास से एकाग्र हो जायेगा।
हठयोग में आठ प्रकार के प्राणायामों का वर्णन है, ये निम्नानुसार है:
१. सूर्य भेद २. उज्जाई
३. सीत्कारी ४. शीतली
५. भस्त्रिका ६. भ्रामरी
७. मूर्छा ८. प्लाविनी
कुछ पुस्तकों में प्लाविनी को आठवाँ कुंभक बताया गया है। कपालभाति षटकर्मों में आता है। मैंने इसका अगले अध्याय में वर्णन किया है । यह प्राणायाम का एक प्रकार है। प्रातःकाल एवं सायंकाल में नित्य अभ्यास हेतु मैं सुखपूर्वक प्राणायाम बता रहा हूँ। तत्पश्चात् मैं उपरोक्त आठों प्राणायामों की विधि का वर्णन करूँगा।
१. सुखपूर्वक प्राणायाम
पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जायें। आँखें बंद कर लीजिए । अंगूठे से दाहिने नासारंध्र को बंद कर लें। बाँयें नासारंध्र से धीरे-धीरे वायु को भीतर खींचिए। अब अनामिका और कनिष्ठा उंगली की सहायता से बाँयें नासारंध्र को भी बंद कर दीजिए और श्वाँस को जितनी अधिक से अधिक देर सुगमता से रोक सकें, भीतर ही रोकें। फिर धीरे-धीरे श्वाँस को बाहर निकालें । अब पुनःदाँयें नासारंध्र से श्वाँस भीतर लें। इसे दोनों नासारंध्रों को बंद कर जितनी अधिक से अधिक देर सुगमता से रोक सकें, भीतर ही रोकें। तत्पश्चात् अनामिका और कनिष्ठा उंगली को हटा कर बाँयें नासारंध्र से श्वाँस बाहर निकालें । यह एक प्राणायाम हुआ। संस्कृत में श्वाँस भीतर लेने को पूरक कहते हैं, श्वाँस बाहर निकालने को रेचक तथा श्वाँस रोकने को कुंभक कहते हैं । दाहिनी हथेली को फैलायें। अब तर्जनी और मध्यमा उंगली को बंद कर लें, शेष उंगलियाँ खुली रहेंगी। यह प्राणायाम हेतु मुद्रा है। दाहिने नासारंध्र को बंद करने के लिए अंगूठे का प्रयोग किया जाता है और अनामिका और कनिष्ठा उंगली का प्रयोग बाँयें नासारंध्र को बंद करने के लिए किया जाता है ।

आप प्रारंभ में कुछ दिनों तक मात्र पूरक और रेचक करें। थोड़े दिनों के अभ्यास के पश्चात् आप कुंभक भी संयुक्त कर सकते हैं। प्रारंभ में मात्र १० सेकेंड तक कुंभक करें और फिर धीरे-धीरे समयावधि बढ़ायें। पहले आप प्रातः और सायंकाल ५-५ प्राणायाम करें। थोड़े अभ्यास के बाद आप १०-१० प्राणायाम कर सकते हैं। धीरे-धीरे यह संख्या प्रातः २० और सायं २० तक कर दें। शनैः-शनैः और क्रमबद्ध अभ्यास आवश्यक है। पूर्ण कालिक योग साधक दिन में चार बार प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
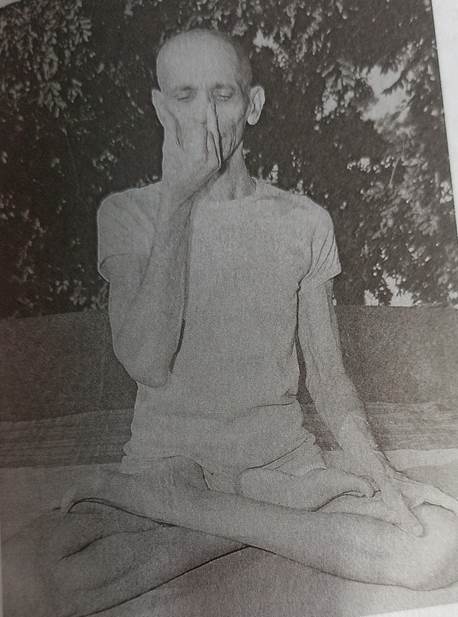
पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात लगा कर १:४: २ होना चाहिए। यदि आप २ सेकेंड तक श्वाँस भीतर लेते हैं, तो श्वाँस को ८ सेकेंड तक रोकें (कुंभक) और ४ सेकेंड में श्वाँस को बाहर निकालें। पूरक, रेचक और कुंभक के समय मानसिक रूप से ॐ का जप करते रहें। ऐसी भावना करें कि सभी दैवी गुण जैसे करुणा, प्रेम, क्षमा, शांति, आनंद आदि भीतर ली जा रही वायु के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और आसुरी दुर्गुण बाहर निकलने वाली श्वाँस के साथ बाहर जा रहे हैं ।
लाभ
प्राणायाम के अभ्यास से शरीर दृढ़ और स्वस्थ बनता है, शरीर की अधिक मात्रा में चर्बी कम हो जाती है, मुख पर तेज आ जाता है। नेत्र हीरे की तरह दमकने लगते हैं। अभ्यासी अत्यंत आकर्षक हो जाता है। उसकी वाणी मधुर हो जाती है। आंतरिक अनाहत ध्वनियाँ स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती हैं । प्राणायाम का अभ्यासी सभी रोगों से मुक्त होता है। वह ब्रह्मचर्य में पूर्ण स्थापित होता है । उसकी भूख बढ़ जाती है, नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है और मन एकाग्र हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। मन प्रबल धारणा हेतु तैयार हो जाता है।
प्राणायाम के अभ्यास के साथ-साथ मौन भी रखें। मिताहार लें, सात्विक आहार लें । धारणा, ध्यान तथा जप हेतु और अधिक समय दें। ठंढे स्थान में निवास करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, इससे आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति शीघ्र जाग्रत हो सकती है तथा आप आनंद, आध्यात्मिक प्रकाश तथा मन की शांति का अनुभव करेंगे। एक उच्च योगी को आठों महत सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।
२. सूर्य भेद प्राणायाम
इस प्राणायाम में पूरक और रेचक मात्र सूर्यनाड़ी अथवा दाँयें नासारंध्र या पिंगला से किया जाता है।
पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जायें। बाँयें नासारंध्र को अपनी दाहिनी अनामिका और कनिष्ठा उंगली से बंद रखें। धीरे-धीरे दाँयें नासारंध्र से बिना किसी प्रकार की ध्वनि किए श्वाँस भरें। जितनी अधिक से अधिक वायु आप भीतर ले सकते हों, लेते हुए दीर्घ श्वसन करें। ठोढ़ी से वक्ष पर दबाव डालते हुए जालंधर बंध लगायें। अंगूठे से बाँयाँ नासारंध्र भी बंद कर दें और श्वाँस को तब तक रोक कर रखें जब तक कि बालों की जड़ में से पसीना न आने लगे । यह सूर्य भेद कुंभक की चरम सीमा है। इस स्थिति में एकदम से नहीं पहुँचा जा सकता है। आपको कुंभक की अवधि में धीरे-धीरे वृद्धि करनी होगी। रेचक करते समय अंगूठे को हटा कर दाँयें नासारंध्र से रेचक करें। आपको श्वाँस एकदम से नहीं वरन् धीरे-धीरे छोड़ना है। पूरक और रेचक बीच में बिना रुके बिना किसी झटके के किया जाना चाहिए।
लाभ
यह प्राणायाम आँतों के कीड़ों तथा रोगों को नष्ट करता है। यह वायु से उत्पन्न होने वाले चार प्रकार के दोषों को दूर करता है तथा वात रोग को ठीक करता है। यह नासाशोथ, सिरदर्द तथा विभिन्न प्रकार के पेशीशूल को दूर करता है। यह नासिका में पाये जाने वाले कीड़ों को दूर करता है। यह क्षय और मृत्यु को नष्ट करता है और कुंडलिनी शक्ति का जागरण करता है। इस प्राणायाम में तीनों बंधों का सुंदर ढंग से अभ्यास होता है। इनके विवरण के लिये बंध त्रय पढ़ें।
३. उज्जाई
पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जाये। मुँह को बंद कर लें। दोनों नासारंध्रों से एक समान गति से तब तक श्वाँस भरें जब तक कि फेफड़े पूरी तरह न भर जायें । जब पूरक करेंगे तो हल्की ध्वनि होगी। दोनों नासारंध्रों को बंद करें, ठोढ़ी से वक्ष पर दबाव डालते हुए जालंधर बंध लगायें। श्वाँस को जितनी अधिक से अधिक देर सुगमता से रोक सकें, भीतर ही रोकें। फिर धीरे-धीरे बाँयें नासारंध्र से श्वाँस को बाहर निकालें।
यह प्राणायाम आप खड़े रह कर भी कर सकते हैं। घेरण्ड संहिता में वर्णन है कि पूरक करने के बाद फेफड़ों और मुंह के द्वारा वायु को खींचें, भरें और तत्पश्चात् मुँह से बाहर निकालें ।
यह क्रिया सिर की गर्मी को दूर करती है। इसका अभ्यासी अत्यंत आकर्षक हो जाता है । उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है। इसके अभ्यास से अस्थमा, क्षयरोग और सभी प्रकार के फेफड़ों के रोग ठीक हो जाते हैं। जरा और मृत्यु को नष्ट करने के लिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। आप प्रातः और सायंकाल चार बार अभ्यास कर सकते हैं।
४. सीत्कारी
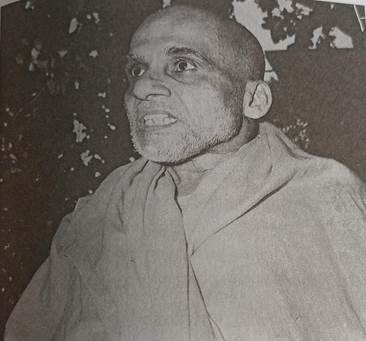
जीभ को मोड़ कर इसकी नोंक को तालु से स्पर्श करायें। मुँह को थोड़ा खुला रखें और मुँह से धीरे-धीरे श्वाँस लें। यदि आपको जीभ में कष्ट हो तो आप इसे ओठों के बीच रखें और मुँह से श्वाँस लें। पूरक करते समय आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। पूरक करने के पश्चात् नासारंध्रों से श्वाँस को बाहर निकालें। यह अभ्यास अभ्यासी के सौंदर्य तथा बल में वृद्धि करता है । यह भूख, प्यास, आलस्य एवं निद्रा को दूर करता है। जब आपको प्यास लगी हो तो इसका अभ्यास कीजिए, आपको प्यास से तत्क्षण आराम मिलेगा। आप इसका दस बार भी अभ्यास कर सकते हैं। आप इसका अभ्यास बैठे हुए और खड़े रह कर भी कर सकते हैं।
५. शीतली प्राणायाम
जीभ को लंबाई में मोड़ें। इसे ओठों से थोड़ा बाहर निकाल लें (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है)। सी की ध्वनि करते हुए मुँह से तेज़ी से श्वाँस भरें। जितनी देर तक आराम से श्वाँस को रोक सकते हों रोकें, उसके पश्चात् दोनों नासारंध्रों से धीरे-धीरे बाहर निकाल दें। इसका अभ्यास बैठे हुए, खड़े हुए अथवा लेटे-लेटे भी दस से पंद्रह मिनट तक भी किया जा सकता है।
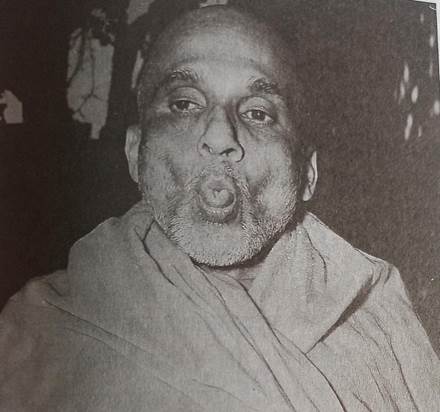
यह प्राणायाम रक्त का शोधन करता है। यह प्यास को शांत करता है और भूख को तुष्ट करता है। यह शरीर को ठंढा रखता है और गुल्म, प्लीहा, विभिन्न असाध्य रोगों, ज्वर, क्षय, अपच, पैत्तिक रोग तथा अन्य रोगों को दूर करता है। इस प्राणायाम का दीर्घकाल तक अभ्यास करते रहने से रक्त इतना अधिक शुद्ध हो जाता है कि एक जहरीला सर्प भी शरीर को हानि नहीं पहुँचा सकता। जब आपको प्यास का अनुभव हो, शीतली का अभ्यास कीजिए। आपको तुरंत प्यास से राहत मिलेगी ।
६. भस्त्रिका
संस्कृत में भस्त्रिका का अर्थ है, धौंकनी। जिस प्रकार लुहार अपनी धौंकनी को एक समान रूप से जल्दी-जल्दी धौंकता है, इसमें आपको उसी प्रकार श्वाँस को लेना है। जल्दी-जल्दी बलपूर्वक श्वाँस छोड़ना भस्त्रिका का लक्षण है।
पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जायें। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें। हथेलियों को घुटनों पर रखें। मुँह को बंद कर लें। अब लुहार की धौंकनी की तरह २० बार जल्दी-जल्दी श्वाँस लें और छोड़ें। सीने को भी बार-बार फैलायें और संकुचित करें। आप कंठ द्वार को भी थोड़ा संकुचित कर सकते हैं। श्वाँस का जल्दी-जल्दी रेचन करने से स्वाभाविक ही श्वास जल्दी से भीतर की ओर खिंचती है। २० पूरक और रेचक करने के बाद एक गहरी श्वाँस लें। श्वाँस को जितनी अधिक-से-अधिक देर सुगमता से रोक सकें, भीतर ही रोकें। फिर धीरे-धीरे दोनों नासारंध्रों से श्वाँस को बाहर निकालें । २० रेचक से एक चक्र होता है। आप प्रातः और सायं ३ या ४ चक्र कर सकते हैं। प्रारंभ में एक चक्र में मात्र १० रेचक करें, फिर धीरे-धीरे इनकी संख्या २० तक बढ़ायें। यह प्राणायाम खड़े हो कर हाथों को जाँघों पर रख कर भी किया जा सकता है।
कुछ लोग तब तक अभ्यास को खींचते हैं जब तक कि वे थक न जायें। इसको करने पर आपको बहुत पसीना आयेगा । यह अत्यधिक शक्तिशाली क्रिया है । यदि आपको थोड़ा चक्कर जैसा अनुभव हो तो अभ्यास रोक दें और कुछ देर सामान्य श्वसन करें। प्रत्येक चक्र के बाद आप २ मिनट विश्राम कर सकते हैं।
भस्त्रिका गले की सूजन को दूर करता है, जठराग्नि बढ़ाता है, कफ का नाश करता है तथा नासिका और वक्ष के सभी रोगों को दूर करता है तथा दमा रोग को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसके अभ्यास से अच्छी भूख लगती है। यह अभ्यासी को कुंडलिनी जागरण के योग्य बनाता है। इससे वात, पित्त और कफ की अधिकता से उत्पन्न होने वाले सभी रोग दूर हो जाते हैं। यह शरीर को पर्याप्त मात्रा में गर्मी प्रदान करता है। यह नाड़ियों को शुद्ध करता है। यह सभी कुंभकों में से सर्वाधिक लाभदायक है । भस्त्रिका का अभ्यास अवश्य ही किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्राण को सुषुम्ना में स्थित तीनों ग्रंथियों के भेदन योग्य बनाता है। इसका अभ्यासी सदा स्वस्थ रहता है। रेचक अथवा चक्रों की संख्या का निर्णय अभ्यासी की शक्ति अथवा क्षमता द्वारा किया जाता है। आपको अति नहीं करना चाहिए। ॐ का जप भाव सहित मानसिक रूप से करें। भस्त्रिका के अन्य भी प्रकार है जिनमें पूरक और रेचक हेतु बारी-बारी से नासारंध्रों को बदल-बदल कर प्रयोग किया जाता है।
७. भ्रामरी
पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठें। नर मधुमक्खी की तरह आवाज करते हुए दोनों नासारंध्रों से जल्दी-जल्दी श्वाँस भीतर लें और मादा मधुमक्खी की तरह आवाज करते हुए दोनों नासारंध्रों से जल्दी-जल्दी श्वाँस बाहर निकालें । घेरण्ड संहिता में भ्रामरी का अलग प्रकार से वर्णन किया गया है।
अधिक देर सुगमता से रोक सकें, भीतर ही रोकें। फिर धीरे-धीरे दोनों नासारंध्रों से श्वाँस को बाहर निकालें। इसका अभ्यास एकांत स्थान में रात के समय जब बिल्कुल शांति हो, किया जाना चाहिए उस समय आप अनाहत ध्वनि स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे। इस कुंभक के अभ्यासी को जो आनंद प्राप्त होता है, वह असीम और अवर्णनीय है। इस कुंभक में सफलता मिलने पर योगी को समाधि प्राप्त होती है।
८. मूर्छा
अपने आसन पर बैठ जायें और गहरी श्वाँस लें। ठोढ़ी को छाती पर लगा कर जालंधर बंध लगा कर श्वाँस को तब तक रोके, जब तक कि आपको मूर्छा का अनुभव न होने लगे। तत्पश्चात् अत्यंत धीरे-धीरे श्वाँस बाहर निकालें। यह मूर्छा कुंभक मन को ज्ञानशून्य बनाता है और इस कारण प्रसन्नता प्रदान करता है। घेरण्ड संहिता में इस क्रिया का वर्णन इस प्रकार किया है : "सुखेन कुंभकम्"-श्वाँस को जितनी देर सुखपूर्वक रोक सकें, भीतर ही रोकें। आपको इस अवधि में अपनी सामर्थ्य से अधिक वृद्धि नहीं करनी चाहिये। जब इस कुंभक का अभ्यास किया जाता है, तो मन को आत्मा पर लगायें । जब मन की लंबे समय तक गहन धारणा की जाती है तो यह ज्ञानशून्य हो जाता है और आपको आनंद और खुशी का अनुभव होता है।
९. प्लाविनी
इस प्राणायाम के अभ्यास से व्यक्ति जल के ऊपर कमल की भाँति तैर सकता है। कंठ द्वार को बंद करके वायु को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में निगलें और पेट को पूर्ण रूपेण भरें। यदि आपका पेट वायु से पूरी तरह भरा हो, उस समय पेट को थपथपाने पर एक विशेष प्रकार की आवाज आयेगी। पेट और फेफड़ों को वायु से भरने के द्वारा व्यक्ति बड़े ही आराम और सरलता से घंटों तक जल के ऊपर तैर सकता है। धीरे-धीरे डकार ले कर अथवा उड्डियान बंध द्वारा पेट में से गैस को बाहर निकालना चाहिये। यदि आप इस क्रिया में प्रवीण व्यक्ति द्वारा वायु निगलने की विधि को देखें तो आपको इस प्राणायाम की क्रिया विधि एकदम स्पष्ट होगी। जो इस प्लाविनी कुंभक का अभ्यास करता है, वह भोजन के बिना मात्र वायु पर कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है।
१०. केवल कुंभक
कुंभक दो प्रकार के होते हैं—सहित कुंभक और केवल कुंभक। जो कुंभक पूरक और रेचक के साथ संयुक्त रहता है, उसे सहित कुंभक कहते हैं। तथा जो इनके बिना रहता है, उसे केवल कुंभक कहते हैं।
पहले सहित कुंभक में दक्षता प्राप्त कीजिए, तत्पश्चात् केवल कुंभक का अभ्यास कीजिए। दोनों नासारंध्रों से पूरक करने के पश्चात् कुंभक का अभ्यास करें (घेरण्ड संहिता : ५/९२) । आप २-३ घंटों में भी एक बार इस कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे-धीरे कुंभक की अवधि बढ़ाने का प्रयास करें। केवल कुंभक में कोई रेचक पूरक नहीं होता है। आपको कुंभक की अवधि बढ़ाने का प्रयास करना होगा। कुंभक के समय आपको मन को सभी विषयों से हटाना चाहिए और इसे आत्मा अथवा भ्रूमध्य में दृढ़ता पूर्वक लगाना चाहिए। केवल कुंभक के अभ्यास से अभ्यासी को राजयोग की स्थिति प्राप्त होती है । इस कुंभक के अभ्यास से उसे कुंडलिनी का ज्ञान होता है। लंबे समय तक इस कुंभक के अभ्यास से अभ्यासी जितनी देर तक चाहे श्वाँस को रोक सकता है, उसकी कुंडलिनी जाग्रत होती है और सुषुम्ना सभी ग्रंथियों से मुक्त हो जाती है। यह कुंभक दीर्घायु प्रदान करता है और सभी रोगों को नष्ट करता है। जो केवल कुंभक जानता है, वह सच्चा योगी है।
अध्याय ३
मुद्रा और बंध
१. महा मुद्रा
गुदा द्वार को बाँय एड़ी से दबायें और दाँयें पैर को सीधा रखें। धीरे से आगे की ओर झुकें और हाथों से अपने दाँयें पंजे को पकड़ें। श्वाँस भीतर लें और रोक कर रखें। ठोढ़ी को वक्ष पर दबायें और जालंधर बंध लगायें।
दृष्टि को त्रिकुटि पर रखें। जितनी देर तक सरलता पूर्वक रोक सकें, श्वाँस को रोकें। तत्पश्चात् धीरे-धीरे सिर और शरीर को उठायें और श्वाँस को बाहर निकाल दें। इसी प्रकार इसे ४ से ६ बार दोहरायें। तत्पश्चात् विपरीत ओर से गुदा द्वार को दाँयें पैर की एड़ी से गुदा को दबा कर और बाँयें पंजे को पकड़ कर करें।
लाभ
यह क्षय, बवासीर, प्लीहा वृद्धि, अपच, जठरशोथ, कब्ज, ज्वर आदि को दूर करती है। इसके अभ्यास से जीवन काल में वृद्धि होती है। यह अभ्यासी को महान् सिद्धियाँ प्रदान करती है।
यह जानुशिरासन की तरह है, अंतर मात्र इतना है कि जानुशिरासन में आपको रेचक करके फिर झुकना होता है और सिर घुटनों तक पहुँचना चाहिए। यह थोड़ा-थोड़ा अर्ध पश्चिमोत्तानासन की भाँति है।
२. ताड़न क्रिया
पद्मासन में बैठ जायें। हथेलियों को भूमि पर जमा कर, इनके बल पर अपने शरीर को उठायें और नितंबों को जल्दी-जल्दी दस या बीस बार भूमि पर पटकें । अभ्यास के समय कुंभक लगाये रहें। इसे २ या ३ बार दोहरायें और इसकी संख्या में शनैः-शनैः वृद्धि करें। इस क्रिया को करने से कुंडलिनी शीघ्र जाग्रत होती है।
३. महा बंध
बाँयीं एड़ी को गुदा में अथवा कंद (गुदा से २ इंच ऊपर और जनन अंगों से २ इंच नीचे) के ऊपर लगायें। दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा कर घुटने के ऊपर रखें और बंध त्रय (मूल बंध, उड्डियान बंध और जालंधर बंध) का अभ्यास करें। मूलाधार में सुषुम्ना पर धारणा करें। १० बार प्राणायाम का अभ्यास करें। तत्पश्चात् दाहिनी एड़ी को गुदा अथवा कंद पर रखें और बाँयाँ पैर दाहिनी जंघा पर रखें और बंध त्रय के साथ १० बार प्राणायाम करें। सामान्यतया योगी महा मुद्रा, ताड़न क्रिया, महा बंध और महा वेध करता है। यह एक अच्छा संयोजन है और ऐसा करने से ही अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं। महा बंध जरा और मृत्यु का नाश करता है और इसके अभ्यास से योगी की सभी इच्छायें पूर्ण होती हैं। इस बंध के लाभ बंध त्रय के समान ही हैं, लेकिन महा बंध शीघ्र कुंडलिनी जागरण करता है।
४. महा वेध
महा वेध ताड़न क्रिया एवं बंध त्रय का संयुक्त रूप है। महा बंध की स्थिति में बैठें। दोनों नासारंध्रों से श्वाँस भीतर लें और जालंधर बंध लगा कर श्वाँस को रोकें । अब हथेलियों को भूमि पर रखें, शरीर को उठायें और नितंबों को १० २० बार हल्के से भूमि पर पटकें। इसको करते समय आप पैरों को अपने स्थान से हिलने न दें। जैसे आप महा बंध में रखते हैं, उस तरह पैरों को गुदा पर रखने से आप संपूर्ण शरीर को वैसे का वैसा ही नहीं उठा सकते हैं। इसलिये महा वेध के लिये आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। इसके अभ्यास से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। जब आपको थकान का अनुभव हो अथवा मूर्छा आने लगे तो अत्यंत धीरे-धीरे पूरक करें। प्रारंभ में प्रत्येक बैठक में मात्र एक बार इसे करें, बाद में धीरे-धीरे संख्या में वृद्धि करें। इसका अभ्यास अपने गुरु की उपस्थिति में करें। इसका अभ्यास ताड़न क्रिया और महा बंध के पश्चात् किया जाना चाहिए। यह शरीर की समस्त दुर्बलता को दूर करता है और कुंडलिनी का जागरण करता है।
५. योनि मुद्रा
सिद्धासन में बैठ जायें। गहरी श्वाँस ले कर कानों को दोनों अंगूठों से बंद कर लें। आँखों को दोनों तर्जनियों से, नासारंध्रों को मध्यमा उंगलियों से, ऊपरी ओंठ को अनामिका उंगली से तथा निचले ओंठ को कनिष्ठा उंगली से बंद करें।
यह जप करने के लिये उत्तम मुद्रा है। इसे बद्धयोनि मुद्रा कहते हैं। आपको इस मुद्रा की प्रविधि गुरु से प्रत्यक्ष रूप में सीखनी चाहिए। आपको छहों चक्रों तथा कुंडलिनी पर ध्यान करना चाहिए और साथ ही बीज मंत्र का जप और प्राणायाम करना चाहिए। इस मुद्रा को सफलता पूर्वक करने के लिये आपको ब्रह्मचर्य में पूर्ण स्थित होना चाहिए । “देवानामपि दुर्लभा " '—यह देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। एक बार इस मुद्रा में सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगाभ्यासी योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है।
६. योग मुद्रा
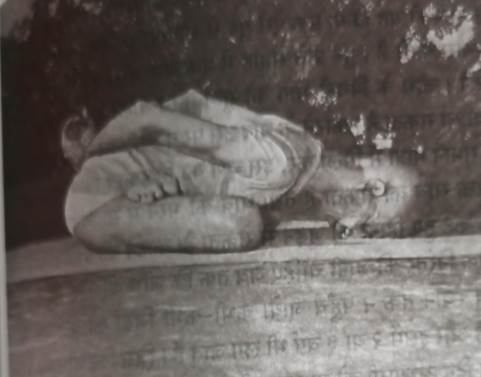
पद्मासन में बैठ जायें। हाथों को घुटनों पर रखें। अब रेचक करें और तब तक आगे झुकें जब तक कि आपका सिर भूमि को स्पर्श न करने लगे। यदि आप इस आसन में लंबे समय तक रुकें तो आप सामान्य रूप से श्वाँस ले सकते हैं अथवा बैठी हुई स्थिति में आ जायें और पूरक करें। हाथों को एड़ियों पर रखने के स्थान पर आप उन्हें पीठ की ओर ले जायें और दायें हाथ से बाँयीं कलाई पकड़ें और फिर आगे की ओर झुकें। यह उदर अंगों के लिये बहुत अच्छी क्रिया है।
७. खेचरी मुद्रा
खेचरी मुद्रा में जिह्वा तथा मन आकाश में रहते हैं। 'ख' का अर्थ है आकाश और 'चरी' का अर्थ है चलना । अर्थात इस मुद्रा के अभ्यास से योगी आकाश में विचरण करता है।
इस मुद्रा का प्रारंभिक भाग है जीभ को लंबा करना। जीभ के निचले हिस्से को एक तेज धार वाले चाकू से बाल के बराबर मोटाई में काटा जाता है। आपको यह क्रिया एक ऐसे गुरु से सीखनी चाहिए जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। गुरु प्रति सप्ताह में एक बार जीभ का थोड़ा-थोड़ा भाग काटेंगे। जीभ के निचले भाग को सुन्न करने वाली दवा से संवेदना रहित किया जा सकता है। काटने के बाद उस पर कत्था, नमक और फिटकरी को एक समान मात्रा में मिला कर, इस चूर्ण का छिड़काव किया जा सकता है। यह रक्त स्राव को रोकता है तथा घाव को भरने में सहायता करता है और नमक कटे हुए हिस्से को जुड़ने से रोकता है। काटने की प्रक्रिया प्रति सप्ताह तब तक निरंतर की जानी चाहिए जब तक कि जीभ की नोंक सरलता पूर्वक भ्रूमध्य स्थान तक न पहुँच जाये। कभी-कभी जिह्वा को कई बार काटना होता है और इसमें २ या ३ वर्ष भी लग जाते हैं। जिस दिन जीभ काटी जाती है, उस दिन अभ्यासी को मात्र दूध ही लेना चाहिए। अन्य दिनों में जीभ की ताजे मक्खन से मालिश करनी चाहिए और इसे दिन में कई बार बाहर खींचना चाहिए। इस प्रकार जीभ लम्बी की जा सकती है। यह मुद्रा का प्रारंभिक भाग है ।
पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जायें। दृष्टि को त्रिकुटि में दोनों भौंहों के मध्य स्थिर रखें । जीभ को मोड़ें और इसे तब तक भीतर ले कर जायें जब तक कि जीभ की नोंक से नासारंध्रों का पिछला द्वार बंद न हो जाये। इस मुद्रा के अभ्यास से अभ्यासी मूर्छा, भूख, प्यास और आलस्य से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन काल में वृद्धि हो जाती है। वह कई दिनों और महीनों तक श्वाँस को रोक सकता है। खेचरी मुद्रा करने वाले योगी स्वयं को भूमि के नीचे बंद करके ६ माह पश्चात् भी जीवित बाहर आ जाते हैं। प्राचीन काल में योगी इस मुद्रा की सहायता से वायु गमन किया करते थे।
८. मूल बंध
पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जायें। गुदा द्वार को संकुचित करें। और अपान वायु को ऊपर की ओर खींचें। अपान वायु जो कि मल को बाहर निकालने का कार्य करती है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नीचे की ओर जाने की है। मूल बन्ध के अभ्यास से गुदा द्वार को संकुचित करने से यह अपान वायु बल पूर्वक ऊपर की ओर खींची जाती है और इसे ऊपर की ओर ले जाया जाता है। यह मूल बन्ध कहलाता I
९. जालंधर बंध
नाभि में स्थित जठराग्नि तालु के छिद्र द्वारा सहस्रार चक्र से रिसने वाले अमृत का उपयोग कर लेती है। जालंधर बंध इस अमृत को नाभि में नहीं जाने देता। जालंधर बंध का अभ्यास पूरक के पश्चात् अर्थात श्वाँस रोकते समय (कुंभक) किया जाता है। जालंधर बंध के अभ्यास से प्राण बाहर नहीं जा पाता। कंठ को संकुचित करें और ठोढ़ी को दृढ़ता पूर्वक वक्ष पर दबायें। जब कुंभक की अवधि समाप्त हो जाये तो सिर उठा कर अपनी सामान्य स्थिति में ले आयें और सिर, गर्दन और धड़ एक सीध में करके तत्पश्चात् श्वाँस बाहर निकालें ।
१०. उड्डियान बंध
उड्डियान शब्द संस्कृत के मूल 'उड' और 'डि' शब्द से आया है। जिसका अर्थ है उड़ना । जब इस बंध का अभ्यास किया जाता है तो प्राण सुषुम्ना के द्वारा ऊपर उड़ते हैं। इसलिये इसे उड्डियान कहा जाता है।
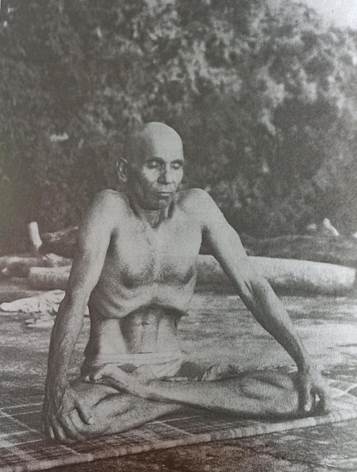
इसका अभ्यास कुंभक के अंत में तथा रेचक के प्रारंभ में किया जाता है। रेचक के समय पेट को थोड़ा पीछे की ओर खींचा जाता है। नाभि के ऊपर और नीचे की आँतें ऊपर की ओर खींची जाती हैं। पेट वक्ष गुहा में बहुत ऊपर पीठ की ओर रहता है। आप इसे प्राणायाम के अभ्यास के समय बैठे हुए अथवा पेट के व्यायाम की तरह खड़े-खड़े कर सकते हैं। इस बंध को ६ से ८ बार दोहरायें। उड्डियान नौलि क्रिया की प्रथम स्थिति है। नौलि क्रिया सामान्यतया खड़े हो कर की जाती है, जब कि उड्डियान बैठ कर भी किया जा सकता है। यह क्रिया ब्रह्मचर्य के पालन में बहुत सहायक है। यह अभ्यासी को सुंदर स्वास्थ्य, बल और शक्ति प्रदान करता है।
जब इसे नौलि के साथ संयुक्त कर दिया जाता है तो यह आमाशय हेतु शक्तिशाली शक्ति वर्धक का काम करता है। योगियों के लिये कब्ज, दुर्बल पाचन शक्ति तथा अन्य आँतों के विकारों से लड़ने के लिये नौलि और उड्डियान शक्तिशाली हथियार हैं। आप इन दोनों क्रियाओं द्वारा आँतों की सभी मांस पेशियों की मालिश कर सकते हैं। इस हेतु अन्य कोई भी क्रियायें इनकी बराबरी नहीं कर सकती हैं। उड्डियान सभी बंधों में सर्वश्रेष्ठ है। असाध्य रोगों में जहाँ सभी दवायें असफल हो जाती हैं वहाँ नौलि और उड्डियान अत्यंत शीघ्र प्रभाव डालते हैं और उनका उपचार करते हैं। नौलि का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया जा रहा है।
११. बंध त्रय
यह मूल बन्ध, जालंधर बंध और उड्डियान बंध का संयुक्त रूप है। इसका अभ्यास सिद्धासन में बैठ कर प्राणायाम करते समय किया जाता है। सभी बंधों की प्रविधि अलग से पूर्व में ही दी जा चुकी है। बंध त्रय के लिए पूरक करते समय गुदा द्वार को संकुचित करें। यह मूल बन्ध है। कुंभक के समय ठोढ़ी से वक्षस्थल पर दबाव डाल कर जालंधर बंध लगायें, तत्पश्चात् सिर उठायें और रेचक करें और पेट को वक्ष गुहा में ऊपर की ओर खींचें । इसे उड्डियान कहते हैं । जब अपान ऊपर उठती है तो यह अग्नि मंडल में पहुँचती है, तत्पश्चात् वायु से प्रज्वलित हो कर अग्नि की ज्वाला ऊँची उठती है। गर्म अवस्था में अग्नि और अपान प्राण साथ एक होते हैं। इस अग्नि के द्वारा सोती हुई कुंडलिनी एक फुंफकार की ध्वनि के साथ जाग्रत हो जाती है तथा उस सर्प की भाँति सीधी हो जाती है जिसे छड़ी से पीटा जा रहा हो और यह ब्रह्मनाड़ी के छिद्र में प्रवेश कर जाती है।
प्रातः और सायंकाल बंध त्रय सहित १० अथवा २० प्राणायाम नित्य करें। सुख पूर्वक प्राणायाम में बताये अनुसार १:४: २ का अनुपात रखें और धीरे-धीरे प्रत्येक बैठक में प्राणायामों की संख्या में वृद्धि करते जायें।
श्वाँस को अपनी सामर्थ्य से अधिक रोकने का प्रयत्न न करें। अभ्यास में श्वाँस में अवरोध का तनिक भी अनुभव नहीं होना चाहिए। आपको पूरक, रेचक और कुंभक के मध्य इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करना चाहिए कि आप समस्त १० अथवा २४ प्राणायाम सरलता पूर्वक और आराम से कर सकें। बंध त्रय पेट की चर्बी को अत्यंत शीघ्र घटाता है। इसके अभ्यास से कुंडलिनी अत्यंत शीघ्र जाग्रत होती है। इसके अभ्यास से मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डियान बंध के सभी लाभ प्राप्त होते हैं।
१२. विपरीत करणी मुद्रा
जब यह मुद्रा प्रदर्शित की जाती है तो यह सर्वांग आसन के समान दिखाई देती है। हमारे शरीर के भीतर सूर्य नाभि के मूल में रहता है और चंद्रमा तालु के मूल में । वह क्रिया जिसके द्वारा इस सूर्य को ऊपर की ओर लाया जाता है और चंद्रमा नीचे की ओर, उसे विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति विपरीत हो जाती है।
भूमि पर लेट जायें। पैरों और जाँघों को धीरे-धीरे ऊपर की ओर 'उठायें। पैरों को सीधे रखें। पैरों को सहारा देने के लिए हथेलियों को कमर के पास रखें। स्थिर रहें। प्रथम दिन इसे मात्र एक मिनट तक करें, तत्पश्चात् धीरे-धीरे इसकी अवधि में वृद्धि करें। इसके अभ्यास से छह माह पश्चात् चेहरे की झुर्रियाँ अदृश्य हो जायेंगी। आप इसका अभ्यास प्रातःकाल २ घंटे और सायंकाल २ घंटे कर सकते हैं। आप इस मुद्रा में अपने इष्ट मंत्र का जप भी कर सकते हैं। जैसे ही मुद्रा समाप्त हो, आप एक प्याला दूध ले सकते हैं। शीर्षासन को भी विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं।
१३. शक्तिचालन मुद्रा
वज्रासन में बैठ जायें दाहिने पैर की एड़ी को दाँयें हाथ से और बाँयें पैर की एड़ी को बाँये हाथ से पकड़ें। पैरों को जमाये रहें। अब नितंबों को उठा कर जितनी बार संभव हो पटकें। अंत में भस्त्रिका प्राणायाम कुंभक के साथ करें। थोड़ा विश्राम करें, तत्पश्चात् अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इसे २ या ३ बार दोहरायें। आप इस मुद्रा का अभ्यास प्रातः और सायंकाल दोनों समय आधा से एक घंटे तक कर सकते हैं। इस अभ्यास से नाड़ियों में प्राण के प्रवाह का अनुभव होता है, नाड़ियाँ शीघ्र शुद्ध हो जाती हैं।
यह मुद्रा कुंडलिनी में स्पंदन करती है। सभी यौगिक क्रियाओं के अभ्यास के समय लंगोटी अथवा कौपीन अथवा छोटी पतली चड्डी पहने रहें, तभी आप उन्हें सरलता से कर पायेंगे।
१४. अश्विनी मुद्रा
वज्रासन अथवा पद्मासन में बैठ जायें। गुदा द्वार को कई बार संकुचित करें और विमोचित। यह कुंडलिनी शक्ति का जागरण करती है। कब्ज दूर करती है। आपको इसके अभ्यास से स्वाभाविक रूप से शौच जाने की इच्छा होगी। आपको खुल कर शौच होगा। मूल बन्ध में गुदा का मात्र संकुचन किया जाता है। अश्विनी मुद्रा में आपको इसे निरंतर संकुचित और विमोचित करते रहना पड़ता है। यही मूल बन्ध और अश्विनी अंतर है। मुद्रा में अंतर है ।
१५. तड़ागी मुद्रा
पश्चिमोत्तानासन में बैठ जाइये। पेट को भीतर करें। इसके लिये आपको रेचक करना होगा। अब पश्चिमोत्तानासन करें, फिर उड्डियान बंध लगायें । यह तड़ागी मुद्रा है। बाद में आप सीधे बैठ जायें और पूरक करें । आप इसे ४ से ६ बार कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन और उड्डियान बंध के सभी लाभ इस मुद्रा से प्राप्त होते हैं। यह पेट का अच्छा व्यायाम है।
१६. भूचरी मुद्रा
पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जाइये। अपनी दृष्टि नासिकाग्र पर केंद्रित करें और गहन ध्यान में डूब जायें। यह भूचरी मुद्रा है।
१७. अगोचरी मुद्रा
मोम की गोली से अपने कानों को बंद कर लें। पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जाइये। गहन धारणा और ध्यान करें। इसके अभ्यास से आपको अनाहत ध्वनि सुनाई देगी। लंबे समय के पश्चात् बिना कानों को बंद किये भी आप अनाहत ध्वनि सुन सकेंगे।
१८. शांभवी मुद्रा
शांभवी मुद्रा तब आती है, जब लक्ष्य आंतरिक होता है और नेत्र स्थिर रहते हैं ।
दृष्टि को भ्रूमध्य में केंद्रित करें। आप स्वाभाविक रूप से ध्यान और समाधि में प्रवेश करेंगे। आपमें अंतरदृष्टि का विकास होगा। जो शांभवी मुद्रा का अभ्यास करता है, वह सच्चा योगी है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा है।
१९. मंडूकी मुद्रा
मुँह को बंद कर लें। जिह्वा को तालु की ओर मोड़ें। सहस्रार से रिसने वाले अमृत का धीरे-धीरे पान करें। यह मंडूकी मुद्रा है। यह खेचरी मुद्रा का प्रारंभिक अभ्यास है। इस मुद्रा से शरीर को चिर-यौवन की प्राप्ति होती है।
२०. भुजंगिनी मुद्रा
गर्दन को थोड़ा आगे की ओर झुका कर, कंठ द्वार को बंद करें। ग्रासनली से वायु का पान करें। यह कुछ-कुछ प्लाविनी प्राणायाम की प्रारंभिक क्रिया की भाँति है। उड्डियान बंध करने से भीतर ली गयी वायु इसको करने से बाहर निकल जायेगी। यह क्रिया अपच तथा अजीर्ण हेतु उत्तम है।
२१. मातंगिनी मुद्रा
कंठ तक पानी में खड़े हो जायें। आप जल के एक बड़े टब का भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा दोनों हाथों में जल भर लें और नासिका से जल को भीतर खींचें और इसे मुँह से बाहर फेंकें, यह व्युत कर्म है। तत्पश्चात् जल को मुँह से खींचें और इसे नासिका से बाहर निकालें। इसे शीत कर्म कहते हैं। इस क्रिया को दोहरायें। सर्दी-जुकाम, नासाशोथ और नासिका के अन्य रोग इससे दूर होते हैं। जिनको सर्दी अत्यंत शीघ्र हो जाती है, वे इसके अभ्यास से सर्दी से पूर्णतया अप्रभावित रहते हैं। (अंत में 'स्वास्थ्य हेतु नासिका से जल पिएँ' शीर्षक में इस क्रिया को विस्तार से बताया गया है।)
२२. वज्रोली मुद्रा
राजा भर्तृहरि तथा बनारस के त्रिलंग स्वामी इस मुद्रा में सिद्ध हस्त थे। आपको इसे किसी ऐसे गुरु से सीखना होगा जो स्वयं इसका अभ्यास करते हों। वर्तमान में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको इस मुद्रा का ज्ञान है। इसकी साधना के समय अभ्यासी एक चाँदी की नलिका को अपनी मूत्र नलिका में प्रवेश कराके उसके द्वारा जल खींचते हैं।
थोड़े अभ्यास के बाद वे इससे दूध खींचते हैं, तत्पश्चात् तेल और फिर शहद खींचते हैं। अंत में वे बिना नली की सहायता के पारा भी खींच लेते हैं। जो योगी इस मुद्रा का अभ्यास करता है, उसके वीर्य की एक बूँद भी बाहर नहीं निकल सकती है। योगी अपने वीर्य को ऊपर खींच कर इसे ओज शक्ति के रूप में संरक्षित रखता है। मूल बन्ध, महा बंध, महा मुद्रा, आसन और प्राणायाम वज्रोली मुद्रा में सहायक होते हैं। वज्रोली मुद्रा का अभ्यास गुरु के प्रत्यक्ष निर्देशन में किया जाना चाहिए।
अध्याय ४
क्रियाएँ
षट कर्म
(छह शोधन क्रियाऐं)
हठयोग में शरीर के शोधन के लिए छह क्रियाऐं निर्दिष्ट की गयी हैं। ये क्रियाऐं मात्र शरीर को बाहर और आंतरिक रूप से स्वच्छ मात्र ही नहीं करतीं, वरन् ये शरीर को शक्तिशाली भी बनाती हैं। इनका नित्य अभ्यास किया जाना चाहिए। ये क्रियाऐं हैं—धौति, बस्ति, नेति, नौलि, त्राटक और कपालभाति ।
१.धौति
शुद्धिकरण दो प्रकार का होता है—बाह्य एवं आंतरिक । आंतरिक शुद्धिकरण कई प्रकार से किया जाता है। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण क्रिया की प्रविधि बतायी जा रही है।
वस्त्र धौति : ३ इंच चौड़ा और १५ फीट लंबा एक मलमल का कपड़ा लें। कपड़े के किनारे अच्छी तरह सिले हुए होने चाहिए, कहीं से भी धागे निकले हुए नहीं होने चाहिए। क्रिया के समाप्त होने के पश्चात् इसे साबुन से धोयें और सदैव स्वच्छ रखें। इसे गुनगुने जल में डुबायें। कपड़े को दबा कर जल से बाहर निकाल लें और एक सिरे से थोड़ा-थोड़ा निगलना प्रारंभ करें। प्रथम दिन मात्र एक फीट निगलें और धीरे से बाहर निकाल लें। धीरे-धीरे आप एक सिरे को दृढ़ता से पकड़े रह कर शेष संपूर्ण कपड़ा निगल सकेंगे। इसे कुछ मिनट के लिए आमाशय में रखें और फिर इसे धीरे से बाहर निकाल दें। कपड़े को बल पूर्वक जल्दी बाहर निकालने का प्रयास न करें। जब क्रिया समाप्त हो जाये तो एक प्याला दूध पियें। यह गले के लिए चिकनाई का कार्य करेगा। जब पेट खाली हो तब इसका अभ्यास करें। इसके लिए प्रातःकाल उत्तम है। इसका अभ्यास ४-५ दिन में एक बार करना पर्याप्त होगा। यह ढीले-ढाले तथा जड़ शरीर वालों के लिये श्रेष्ठ क्रिया है। निरंतर अभ्यास से गुल्म, जठरशोथ, अजीर्ण और अन्य पेट के रोग दूर हो जाते हैं ।
वातसार धौति : जैसा प्लाविनी प्राणायाम में बताया गया है, कंठ द्वार को संकुचित करके वायु को निगलें। इसे पेट में थोड़ी देर रोके रहें। नौलि तथा उड्डियान बंध के अभ्यास से आप निम्न भाग से वायु को ऊपर भेज सकते हैं । वातसार धौति वायु निगलने के द्वारा आंतरिक शुद्धिकरण की एक अन्य विधि है ।
बहिष्कृत धौति : यह वायु के द्वारा आंतरिक अंगों के शुद्धिकरण की विधि है। यह वारिसार धौति के समान है। वायु को आमाशय में बहुत देर तक रोके रहें, फिर इसे निचले भाग से ऊपर की ओर भेजें।
अग्निसार धौति : नाभि को मेरुदंड की ओर दबायें। आँतों तथा पेट को पीछे की ओर खींचें। अब इनको धीरे-धीरे छोड़ें। पुनः भीतर खींचें । इसे १०८ बार दोहरायें। इसे अग्निसार धौति कहते हैं। यह शरीर की अशुद्धियों को दूर करती है। इसके अभ्यास से जीर्ण कब्ज, यकृत शोथ तथा प्लीहा वृद्धि आसानी से दूर हो जाती है। पेट के ऊपर की अतिरिक्त चर्बी अदृश्य हो जाती है। प्रथम दिन पेट को बारह बार भीतर खींचें और बाहर छोड़ें। धीरे-धीरे इसे १०८ बार तक बढ़ायें।
वमन धौति : पेट को जल से पूर्ण रूपेण भरें। कुछ मिनट बाद इसे बाहर निकाल दें। इसके द्वारा पेट की अशुद्धियाँ बाहर फेंक दी जाती हैं। धौति के अन्य प्रकार दाँतों तथा जीभ की स्वच्छता हेतु निर्दिष्ट हैं, जैसे स्नान के द्वारा बाहरी सफाई की जाती है। इनका अभ्यास आप स्वयं नित्य ही करते हैं।
२. बस्ति
बस्ति क्रिया आँतों से कब्ज दूर करने हेतु निर्दिष्ट है। इसके दो प्रकार हैं—स्थल बस्ति और जल बस्ति ।
स्थल बस्ति : भूमि पर बैठ जायें। पैरों को फैला लें। अब अपने हाथों से पंजों को पकड़ लें। यह पश्चिमोत्तानासन के समान है, लेकिन इसमें आपको इतना अधिक आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है कि आपका सिर घुटनों को स्पर्श करने लगे। हाथों से पंजों को पकड़ने के बाद पेट की माँसपेशियों को नीचे की ओर गति देते हुए मथें।
जल बस्ति : यह पूर्व वाली से अधिक प्रभावशाली है। पाँच इंच लम्बी एक बाँस की नली लें। इसका एक सिरा वैसलीन से चिकना कर लें। एक जल से भरे टब अथवा टंकी में जल के भीतर बैठ जायें, जल का स्तर घुटनों तक होना चाहिए। पैरों को भूमि पर रखें। अपने शरीर को पंजों पर संतुलित करें। यह वज्रासन की भाँति है, लेकिन इसमें घुटने उठे रहते हैं और शरीर पंजों पर टिका रहता है। अब गुदा को संकुचित करके अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें। बाँस की नली से जल को आँतों में खींचें। पेट की माँसपेशियों को मथें और जल को बाहर निकाल दें। इसका अभ्यास आँतों के संक्रमण को दूर करने के लिये कभी-कभी करना चाहिए। जो अश्विनी मुद्रा के अभ्यास के द्वारा जल भीतर नहीं खींच सकते, वे एनिमा सिरिंज का प्रयोग कर सकते हैं।
३. नेति
अस्वच्छ नासारंध्रों के कारण आपकी श्वसन क्रिया अनियमित हो जाती है और इस कारण आप बीमार हो सकते हैं। नेति क्रिया नासारंध्रों की स्वच्छता हेतु निर्दिष्ट है ।
एक मजबूत धागे का टुकड़ा लें। इसमें कहीं भी गाँठ नहीं होनी चाहिए। इसका एक सिरा नासिका के भीतर डालें और दूसरा सिरा दृढ़ता से पकड़े रहें। गहरी श्वाँस लेने से आप इस धागे को भीतर खींच सकेंगे। फिर इसे धीरे से बाहर खींच लें। इसे दोनों ओर से करें। इससे आपके दोनों नासारंध्र अच्छी तरह साफ हो जायेंगे । मातंगिनी मुद्रा करें। यह भी नेति क्रिया का ही एक रूप है।
४. नौलि
नौलि क्रिया उदर के भीतरी अंगों एवं पाचन तंत्र के पुनर्नवीनीकरण, शक्तिवर्धन तथा उत्तेजना प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट है। नौलि क्रिया हेतु आपको उड्डियान बंध का ज्ञान होना आवश्यक है। उड्डियान बंध का अभ्यास बैठ कर भी किया जा सकता है, जब कि नौलि क्रिया सामान्यतया खड़े हो कर की जाती है। इन दोनों के मध्य यही अंतर है
दोनों पैर दूर-दूर रख कर खड़े हो जायें। हाथों को जंघाओं पर रखें जिससे पीठ थोड़ी झुक जाये। मुँह के द्वारा तेजी से बल पूर्वक रेचक करें और फेफड़ों को खाली कर दें। पेट की माँसपेशियों को संकुचित करें और बलपूर्वक पीठ की ओर खींचें। यह उड्डियान बंध है। यह नौलि की प्रथम स्थिति है ।
इसके बाद पेट के दाहिने भाग एवं बाँयें भाग को संकुचित करके उदर मध्य भाग को ढीला रखें। इस समय आपके पेट की सभी माँसपेशियाँ एक लंबवत् रेखा में होंगीं। इसे मध्यमा नौलि कहते हैं। जितनी देर तक आराम से रुक सकें, इसी स्थिति में रुके। कुछ दिनों तक मात्र इसी का अभ्यास करना चाहिए ।
इसके बाद आपको पेट के दाँयें हिस्से को संकुचित करना है और ढीला छोड़ना है। इसे वाम नौलि कहते हैं। अब बाँयीं ओर की माँसपेशियों को संकुचित करें और दाँयें भाग को ढीला रखें। इसे दक्षिण नौलि कहते हैं। अभ्यास करते-करते धीरे-धीरे आप पेट की मध्य, दॉय और बाँयी ओर की माँसपेशियों को संकुचित करने की विधि समझ जायेंगे। आपको इस पर भी ध्यान देना है कि वे एक ओर से दूसरी ओर कैसे जाती है ? एक सप्ताह तक इसी का अभ्यास करें।
अब माँसपेशियों को मध्य में रखें। अब इन्हें गोल-गोल घुमाते हुए पहले दाहिनी ओर तत्पश्चात् बाँयीं ओर ले कर जाना है। इसके बाद इनको पहले बाँयीं ओर फिर दाहिनी ओर ले कर जाना है। आपको माँसपेशियों को सदा गोलाकार घुमाना है। अभ्यास में निपुण होने के पश्चात् आप इसे जल्दी-जल्दी भी कर सकेंगे; किंतु आपको इसके लाभ तभी प्राप्त होंगे जब आप इसे धीरे-धीरे करेंगे। नौलि की इस अंतिम स्थिति में उदर की माँसपेशियाँ जब अलग-अलग होती हैं और एक ओर से दूसरी ओर घूमती हैं तो ऐसा लगता है, जैसे मंथन हो रहा हो।
प्रारंभिक अभ्यासी जब दक्षिण नौलि करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा बाँर्यी ओर झुकना चाहिए और बाँयीं ओर की माँसपेशियों को संकुचित करना चाहिए । जब वे वाम नौलि करना चाहें तो उनको थोड़ा दाँयी ओर झुकना चाहिए । मध्यमा नौलि करते समय उनको दोनों ओर से संकुचन के द्वारा संपूर्ण माँसपेशियों को आगे की ओर धक्का देना चाहिए।
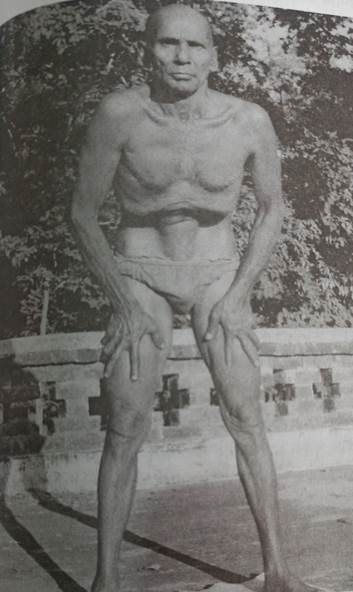
नौलि क्रिया जीर्ण कब्ज, अजीर्ण तथा पाचन तंत्र के अन्य रोगों को दूर करती है। इसके अभ्यास से उदर के अन्य सभी अंग अन्य सुचारु रूप से कार्य करने लगते हैं और इससे यकृत और अग्न्याशय की मालिश होती है। नौलि मानव जाति के लिये वरदान स्वरूप है। यह एक आदर्श रामबाण औषधि है।
५. त्राटक
किसी बिंदु विशेष को अपलक स्थिर दृष्टि से देखना त्राटक कहलाता है। त्राटक मुख्य रूप से धारणा के विकास तथा मन को केंद्रित करने के लिये निर्दिष्ट है। यह हठयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग और राजयोग के साधकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। मन के नियंत्रण के लिये इससे अधिक उपयोगी अन्य कोई विधि नहीं है। पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जाइये। आप कुर्सी पर भी सीधे बैठ सकते हैं। अपने इष्ट देवता, ॐ का चित्र अथवा एक सफेद कागज पर काला बिंदु—इनमें से किसी एक को अपने सामने रखें। बिंदु अथवा चित्र को स्थिर दृष्टि से देखते रहें। आप एक चमकते हुए तारे अथवा घी के दिए की लौ पर भी त्राटक कर सकते हैं। नासिकाग्र अथवा भ्रूमध्य पर दृष्टि को केंद्रित करना भी त्राटक कहलाता है। अपनी आँखें बंद कर लें और विषय को मानसिक रूप से देखने का प्रयास करें। इसका २ मिनट तक अभ्यास करें और शनैः-शनैः समय में वृद्धि करें।
त्राटक के अभ्यास से नेत्र ज्योति में सुधार होता है, नेत्र रोग दूर हो जाते हैं । कई लोगों ने त्राटक का कुछ दिनों तक अभ्यास करने पर अपने चश्मे उतार के फेंक दिये । त्राटक धारणा शक्ति का उच्च स्तर तक विकास करता है।
६. कपालभाति
यह क्रिया कपाल और फेफड़ों के शुद्धिकरण के लिए है। 'कपाल' का अर्थ है सिर और 'भाति' का अर्थ है चमकाना। इस क्रिया के अभ्यास से कपाल चमकने लग जाता है।
पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जाइये । नेत्र बंद कर लें जल्दी-जल्दी पूरक-रेचक करें। इसका अभ्यास तेज़ी से करें, आपको इसमें बहुत अधिक पसीना आयेगा। यह फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा व्यायाम है। जो कपालभाति करने में प्रवीण होते हैं, वे सरलता से भस्त्रिका कर सकते हैं। उदर की माँसपेशियों को संकुचित करके रेचक बलपूर्वक किया जाना चाहिए। प्रारंभ में प्रति चक्र २० रेचक करें और इसमें धीरे-धीरे वृद्धि करते हुए इनकी संख्या १२० तक कर दें । कपालभाति में कुंभक नहीं होता । कपालभाति श्वसन तंत्र तथा नासिका को स्वच्छ करता है। यह श्वसन नलिकाओं के संकुचन को दूर करता है, जिसके फलस्वरूप अस्थमा में आराम होता है और थोड़े समय बाद यह दूर हो जाता है। इसके अभ्यास से फेफड़ों के शिखाग्रों को पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु प्राप्त होती है और क्षय रोग पूर्ण रूप से दूर हो जाता है। इसके अभ्यास से रक्त की अशुद्धियाँ बाहर फेंक दी जाती हैं और परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र में अच्छा सुधार होता है।
कपालभाति का एक और प्रकार है, इसमें दाहिने नासारंध्र से पूरक करते हैं और दाहिने से ही रेचक करते हैं। पुनः दाहिने से पूरक करें और बाँयें से रेचक करें। नेति क्रिया और मातंगिनी मुद्रा में वर्णित शीत कर्म तथा व्युत कर्म भी कपालभाति के ही रूप हैं।
अध्याय ५
योग में ऊर्ध्वारोहण
१. कुंडलिनी
कुंडलिनी वह आद्य शक्ति है जो कि मूलाधार में सुप्त ध्रुवीय अवस्था में रहती है। कुंडलिनी योग वह योग है, जिसमें कि योगी कुंडलिनी का जागरण करता है और निम्न छह चक्रों के भेदन द्वारा इसे सहस्रार की ओर ले जाता है। वह निर्विकल्प समाधि द्वारा सर्वोच्च ज्ञान तथा आनंद प्राप्त करता है। सिर के शीर्ष में भगवान शिव से शक्ति का मिलन होता है।
कुंडलिनी मूलाधार में स्थित त्रिकोण में स्वयंभू लिंग के ऊपर विश्राम कर रही है। इसके तीन कुंडल इसके तीनों गुणों को तथा आधा कुंडल विकृतियों को अभिव्यक्त करते हैं।
सुषुम्ना कंद के मध्य से निकल कर सिर की ओर जाती है। कंद का अर्थ है गाँठ । कंद सभी नाड़ियों का मूल है। गुदा से २ अंगुल ऊपर तथा जननांग से दो अंगुल नीचे कंद स्थित है। यह आकार में चिड़िया के अंडे के समान है। यह चार अंगुल चौड़ा है। इससे ७२००० नाड़ियाँ निकलती हैं। सभी नाड़ियों में से इडा, पिंगला और सुषुम्ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।
मेरुदंड के दाहिनी और बाँयीं ओर से क्रमश: इडा और पिंगला नाड़ियाँ निकलती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ बाँयें से दाँयीं ओर एकांतरित रूप से जाती हैं। ये विभिन्न चक्रों में से हो कर जाती है और भ्रूमध्य में सुषुम्ना के साथ मिल कर त्रिवेणी बनाती हैं। यहाँ से वे नासारंध्रों की ओर चली जाती हैं। जो दाहिने अण्डकोष से आती है, वह बाँयें नासारंध्र को जाती है तथा जो बाँयें अण्डकोष से आती है, वह दाहिने नासारंध्र को जाती है। इडा चंद्र नाड़ी है, यह शीतल है। पिंगला सूर्य नाड़ी है, यह उष्ण है।
मूलाधार चार पंखुड़ियों वाला कमल है। कुंडलिनी यहाँ साढ़े तीन कुंडल मारे हुए निवास कर रही है। मूलाधार छहों चक्रों का मूल है, इसी कारण इसका नाम मूलाधार है।
कुंडलिनी मूलाधार चक्र में इस प्रकार दीप्तिमान होती है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। इस चक्र का तत्व है, पृथ्वी । डाकिनी शक्ति यहाँ निवास करती है। इस कमल के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा हैं। यह पृथ्वी का क्षेत्र है। इसका बीज मंत्र है लं ।
स्वाधिष्ठान दूसरा कमल है जो सुषुम्ना में जननांगों के मूल में स्थित है। इसकी छह पंखुड़ियाँ हैं। इसका तत्व है जल और बीज मंत्र है वं। यह वरुण-बीज हैं। राकिनी देवी यहाँ निवास करती हैं। यह जल का क्षेत्र है। इस कमल के अधिष्ठाता देवता विष्णु हैं।
तीसरा कमल है मणिपूर । यह नाभि के मूल में स्थित है। इसकी दस पंखुड़ियाँ हैं । यह अग्नि तत्व का स्थान है। लाकिनी शक्ति यहाँ निवास करती है । इस कमल के अधिष्ठाता देवता शिव हैं।
अनाहत चौथा चक्र है। यह हृदय में स्थित है। इसकी १२ पंखुड़ियाँ हैं। यह वायु का क्षेत्र है। इसका बीज मंत्र है रं। काकिनी शक्ति यहाँ निवास करती है। इस कमल के अधिष्ठाता देवता ईशा हैं।
पाँचवाँ चक्र है विशुद्ध। यह गले में स्थित है। इसकी १६ पंखुड़ियाँ हैं । यह आकाश का क्षेत्र है। इसका बीज मंत्र है हं। शाकिनी शक्ति यहाँ निवास करती है। इस कमल के अधिष्ठाता देवता सदाशिव हैं।
आज्ञा छठवाँ चक्र है। यह त्रिकुटि में स्थित है। इसकी २ पंखुड़ियाँ हैं। यह मन का स्थान है। हाकिनी शक्ति यहाँ निवास करती है। इस कमल के अधिष्ठाता देवता शंभु हैं। यह प्रणव का क्षेत्र है। सहस्रार चक्र सहस्र पंखुड़ियों वाला चक्र है। यह सिर के शीर्ष में स्थित है। परम शिव यहाँ निवास करते हैं। कुंडलिनी सहस्रार में शिव से एक होती है। यह निर्विकल्प समाधि का परिणाम होता है। समाधि में सहस्रार में शिव और शक्ति के मिलन से प्रवाहित होने वाले अमृत के द्वारा शरीर का पोषण होता है। पीयूष ग्रंथि जिसे रहस्यवादियों द्वारा दूरस्थ संवेदी (एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के मन पर प्रभाव डालना) ग्रंथि माना जाता है और इसे आत्मा का स्थान माना जाता है। यह सहस्रार में स्थित है। यह एक जीवंत ग्रंथि हैं। जब यह कार्य करती है तो यह योगाभ्यासी को निर्विकल्प समाधि या चेतनावस्था की प्राप्ति में सहायता करती है।
योगी प्राणायाम, बंध और मुद्रा के अभ्यास के द्वारा सुषुम्ना के द्वार को खोलता है तथा मूलाधार में सोती हुई कुंडलिनी को जगाता है और इसे निचले छहों चक्रों से होते हुए सिर के शीर्ष में स्थित सहस्रार चक्र में ले कर जाता है । ये छहों चक्र कुंडलिनी के विश्राम स्थल अथवा स्थितियाँ हैं । वह मूलाधार में स्थित ब्रह्मग्रंथि, मणिपूर में स्थित विष्णुग्रंथि तथा विशुद्ध में स्थित रुद्रग्रंथि का भेदन करता है। ग्रंथियाँ वे बाधायें हैं जो कुंडलिनी को ऊपर की ओर बढ़ने से रोकती हैं।
कुंडलिनी सहस्रार में अधिक देर तक नहीं रुकती है। इसके वहाँ रुकने की अवधि योगाभ्यासी की शुद्धता, साधना का स्तर तथा आतरिक आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करती है। अनेक अभ्यासी मात्र निम्न चक्रों में ही रुके रहते हैं। वे निम्न चक्रों में जो आनंद प्राप्त करते हैं, उसी में ही फंस जाते हैं और मिथ्या तुष्टि के कारण आगे सहस्रार की ओर बढ़ने का प्रयत्न नहीं करते। निम्न चक्रों के आनंद का रसास्वादन उनके सहस्रार के परम आनंद की प्राप्ति में बाधक है। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति जिसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधायें हैं, वह सोचता है कि यह संसार ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार वह योगाभ्यासी जो निम्न चक्रों तक पहुँच गया हो, वह मिथ्या कल्पना करता है कि वह परम लक्ष्य तक पहुँच गया है और अपनी आगे की साधना बंद कर देता है। सहस्रार में पहुँचने के बाद योगाभ्यासी को यथासंभव कुंडलिनी के सहस्रार में रुकने की अवधि को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।
योगाभ्यासी को सदा अपनी जागरूकता बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वह जड़ समाधि प्राप्त करता है, तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसे किसी प्रकार के आध्यात्मिक आनंद का अनुभव नहीं होगा। उसे इस नकारात्मक अवस्था में प्रवेश करने से बचना चाहिए।
ऊर्ध्वारोहण के समय मन, प्राण, जीव और कुंडलिनी एक साथ ऊपर की ओर बढ़ते हैं । योगाभ्यासी एक चक्र से दूसरे चक्र की ओर बढ़ता है, तो उसे अपने भीतर से सहायता मिलती है, एक रहस्यमय वाणी उसका प्रत्येक चरण पर पथ प्रदर्शन करती है।
उसकी देवी माँ के प्रति अटल श्रद्धा होनी चाहिए। यह माँ ही है, जो उसका पथ प्रदर्शन करती है। यह माँ ही है जो अपने पुत्र को एक चक्र से दूसरे चक्र को ले कर जाती है। वह उसकी अदृश्य रूप से सहायता करती है । वह उसे ऊपर की ओर धक्का देती है। उसके आलिंगन का अनुभव करें। प्रत्येक चरण पर उनकी कृपा का अनुभव कीजिये। उनके साथ एक बालक की भाँति वार्तालाप कीजिए। सरल और निष्कपट रहिए।
उनसे कहें—“देवी माँ, मैं आपका हूँ, आप मेरी आत्मा का आश्रय स्थल और अवलंबन हैं। मेरी रक्षा करें, मेरा पथ प्रदर्शन करें। मुझ पर दया करें।" आपके सभी संदेह दूर हो जायेंगे। वह आपके लिए सब-कुछ करेंगी। उनकी कृपा के बिना आप आध्यात्मिक पथ में तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप सुषुम्ना के ऊर्ध्वारोहण में थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
यदि योगाभ्यासी मूलाधार चक्र का भेदन कर लेता है, तो उसने पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली है। पृथ्वी उसे प्रभावित नहीं कर सकती । यदि वह स्वाधिष्ठान चक्र को पार कर लेता है, तो उसने जल तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। वह भुवः लोक के संपर्क में रहता है। यदि वह मणिपूर चक्र को पार कर लेता है, तो उसने अग्नि पर विजय प्राप्त कर ली है। अग्नि उसे प्रभावित नहीं कर सकती। वह स्वर्ग लोक के संपर्क में रहता है। यदि वह अनाहत चक्र को पार कर लेता है, तो उसने वायु तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। वायु उसे प्रभावित नहीं कर सकती। वह महः लोक के संपर्क में रहता है। यदि वह 'विशुद्ध चक्र को पार कर लेता है, तो उसने आकाश तत्व पर विजय प्राप्त ली है। आकाश उसे प्रभावित नहीं कर सकता। वह ज्ञान लोक के संपर्क में रहता है। यदि वह आज्ञा चक्र को पार कर लेता है, तो वह तपो लोक के संपर्क में रहता है। इसके बाद वह सत्य लोक में प्रवेश करता है। आज्ञा चक्र और सहस्रार के मध्य कुछ अन्य छोटे चक्र हैं जैसे गुरु चक्र, सोम चक्र, ललना चक्र, मनस चक्र आदि ।
कुंडलिनी के सहस्रार में शिव के साथ मिलन के द्वारा प्रचुर मात्रा में अमृत स्रवित होता है। जब यह नीचे आती है तो यह चक्रों को अमृत से स्नान कराते हुए जाती है और इन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। योगी को विभिन्न चक्रों में विभिन्न प्रकार के आनंद और शक्ति का अनुभव होता है। निर्भयता, मन की अविचल स्थिति, निरंतर ध्यान की स्थिति, निष्काम्यता, संतोष, आध्यात्मिक आनंद, शांति, अंतः आध्यात्मिक शक्ति, विवेक, आत्म संयम, मन की एकाग्रता, ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ आस्था, भक्ति, मन की स्थिरता, आसन की स्थिरता, शुद्धता, मोक्ष की प्रबल आकांक्षा, करुणा, मधुर वाणी, नेत्रों में तेज, मुखमंडल पर विशेष तेज तथा आकर्षक व्यक्तित्व—ये सभी वे चिह्न हैं जो यह इंगित करते हैं कि कुंडलिनी जाग्रत है और यह मूलाधार चक्र का भेदन करके सुषुम्ना में प्रविष्ट हो गयी है। सुषुम्ना में जितना अधिक ऊर्ध्वारोहण होगा, उतने ही अधिक आध्यात्मिक अनुभव होंगे और उतने अधिक उपरोक्त गुण और चिह्न देखे जायेंगे । अंत में कुंडलिनी का सहस्रार में अपने स्वामी शिव के साथ मिलन होता है और निर्विकल्प समाधि होती है। योगी को मोक्ष प्राप्त होता है और उसे परम ज्ञान और परमानंद प्राप्त होता है। योगी निम्न चक्रों में प्रलोभित हो जाता है। उसे समस्त सिद्धियों को त्याग देना चाहिए, मात्र तभी वह अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेगा, सिद्धियाँ उसके पथ में बाधक है। यदि वह सिद्धियों के साथ खेलने लगेगा तो वह अपना लक्ष्य चूक जायेगा और उसका पतन हो जायेगा। जो जागरूक और सावधान नहीं है, जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य और विवेक नहीं है, उस योगाभ्यासी के मन को भटकाने के लिए सिद्धियाँ प्रलोभन हैं।
वह फल जो स्वयमेव वृक्ष पर पकता है, वह अत्यधिक मीठा होता है, लेकिन यह पकने में बहुत अधिक समय लेता है। प्रथम श्रेणी की इमारती लकड़ी धीरे-धीरे बढ़ने वाले वृक्षों से प्राप्त होती है। वे वृक्ष कई वर्षों तक धीरे-धीरे बढ़ते हैं। इसलिए इसी प्रकार वह साधक जो दीर्घकाल तक धैर्य और उत्साह के साथ कठोर साधना करता है, पथ में आने वाली बाधाओं के बाद भी आध्यात्मिक साधना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, जो अपनी गल्तियों तथा दुर्बलताओं को स्वीकार करता है और उन्हें अनुकूल विधियों द्वारा दूर करने का प्रयास करता है, वह अपनी कुंडलिनी का जागरण कर लेता है और पूर्ण योगी बन जाता है। आजकल साधक बहुत ही अधैर्यवान हैं। वे थोड़ा प्राणायाम, शीर्षासन और जप करके कुछ महीनों में ही कुंडलिनी जागरण करके पूर्ण योगी बनना चाहते हैं। यदि कोई अशुद्धियों और रोगों से मुक्त हो तो कुंडलिनी स्वयं जाग्रत होगी और उसे लाभ प्राप्त होगा । यदि साधक का हृदय अपवित्र हो और कामनायें उसके मन में दबी हों, ऐसी स्थिति में यदि वह हठयोग द्वारा बलपूर्वक कुंडलिनी का जागरण करे, तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में जाते समय विभिन्न प्रकार प्रलोभन आयेंगे और उसका पतन हो जायेगा, उसके पास इन प्रलोभनों को रोकने के लिए मानसिक शक्ति ही नहीं रहेगी । माँ कुंडलिनी सभी योग साधनाओं में आपका पथ प्रदर्शन करें! उनका आशीर्वाद आप सब के ऊपर हो!
२. कुंडलिनी का जागरण कैसे करें?
कुंडलिनी उस व्यक्ति के द्वारा जाग्रत होती है जो कि कामनाओं से ऊपर उठ जाता है। वह योगी जिसका हृदय शुद्ध हो और मन वासनाओं और कामनाओं से मुक्त हो, वह कुंडलिनी जागरण से लाभान्वित होता है। वह मनुष्य जिसके मन में अनेक अशुद्धियाँ हों, तो यदि वह आसन, प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं द्वारा कुंडलिनी जागरण कर ले तो वह अपने पैर तोड़ लेगा। वह योग की सीढ़ी पर चढ़ने योग्य ही नहीं रहेगा। लोगों को सर्वप्रथम शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, इसके बाद साधना का ज्ञान और एक योग्य निर्देशक प्राप्त करना चाहिए और स्थिर तथा धीरे-धीरे अभ्यास करना चाहिए।
कुंडलिनी का जागरण हठयोगियों द्वारा आसन-प्राणायाम से, राजयोगियों द्वारा मन के प्रशिक्षण से, भक्तों द्वारा भक्ति और पूर्ण आत्म समर्पण से और ज्ञानियों द्वारा विचार से, तांत्रिकों द्वारा मंत्रों से और गुरु की कृपा से स्पर्श, दृष्टि और संकल्प द्वारा होता है। कुंडलिनी का उत्थान और इसका सहस्रार में अपने स्वामी शिव के साथ मिलन समाधि को प्रभावित करता है।
हालाँकि कुंडलिनी शक्ति सर्प के रूप में साढ़े तीन कुंडल मारे हुए है; लेकिन वह अपने भक्तों के समक्ष जिस भी रूप में वे चाहें, किसी भी रूप में प्रगट हो सकती हैं। वे राम, कृष्ण, हरि, शिव, दुर्गा अथवा गायत्री के रूप में प्रगट हो सकती हैं। योगाभ्यासी कुंडलिनी शक्ति को अपने दिव्य चक्षु से वास्तव में देख सकता है।
कुंडलिनी शक्ति के सहस्रार तक जाने के चार रास्ते हैं। सबसे लंबा रास्ता है—पीठ के द्वारा मूलाधार से सहस्रार तक जाना। वह योगी जो इस मार्ग से कुंडलिनी को ले कर जाता है, वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। यह सर्वाधिक कठिन मार्ग है। श्री शंकराचार्य जी में कुंडलिनी इसी मार्ग से गयी थी।
सबसे छोटा मार्ग है—आज्ञा चक्र से सहस्रार तक जाना। तीसरा मार्ग है— हृदय से सहस्रार तक जाना। चौथा मार्ग है— मूलाधार से सहस्रार तक सामने की ओर से जाना ।
यदि योगी आज्ञा चक्र पर धारणा करता है, तो नीचे वाले चक्र स्वयं ही खुल जाते हैं और उन पर विजय प्राप्त हो जाती है।
जिस प्रकार आज्ञा चक्र के नीचे छह चक्र हैं उसी प्रकार आज्ञा चक्र के ऊपर भी छह चक्र हैं, ये हैं—गुरु चक्र, सोम चक्र, मनस चक्र, ललना चक्र आदि।
जब कुंडलिनी जाग्रत होती है, तो साधक गाता है तथा विशेष ध्वनि निकालता है ।
उसे विभिन्न प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं तथा दिव्य गंध का अनुभव होता है। उसे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उसे मूलाधार में एक तेज ज्योति दिखाई देती है, जैसे कि दस हजार सूर्य एक साथ चमक रहे हों ।
वह साधक जो साहसी, समर्पित, विनम्र, विवेकी, दयालु, शुद्ध और वैराग्यवान है, वह सरलता पूर्वक कुंडलिनी जाग्रत कर सकता है ।
जब कुंडलिनी जाग्रत हो जाती है तो शरीर और शक्तिशाली कंपन होते हैं। मूलाधार में
कुंडलिनी जागरण के पश्चात् प्रकृति स्वयं ही सभी प्रकार की क्रियाएं, आसन, बंध, मुद्रा, प्राणायाम करती है और कुंडलिनी को सहस्रार में ऊपर की ओर धकेलती है।
३. चक्र
|
क्रमाक |
चक्र |
देव |
लोक |
तत्त्व |
पंखुड़ियों की संख्या
|
बीजाक्षर |
|
१ |
मूलाधार |
ब्रह्मा गणपति |
भूः |
पृथ्वी |
४ |
लं |
|
२ |
स्वाधिष्ठान |
विष्णु |
भुवः |
जल |
६ |
वं |
|
३ |
मणिपुर |
रूद्र |
स्व: |
अग्नि |
१० |
रं |
|
४ |
अनाहत |
ईश |
मह: |
वायु |
१२ |
यं |
|
५ |
विशुद्ध |
सदाशिव |
तन: |
आकाश |
१६ |
हं |
|
६ |
आज्ञा |
शम्भू |
तप: |
मन |
२ |
ॐॐ |
|
७ |
सहस्रार |
परमशिव परा-शक्ति |
सत्य |
|
१०० |
|
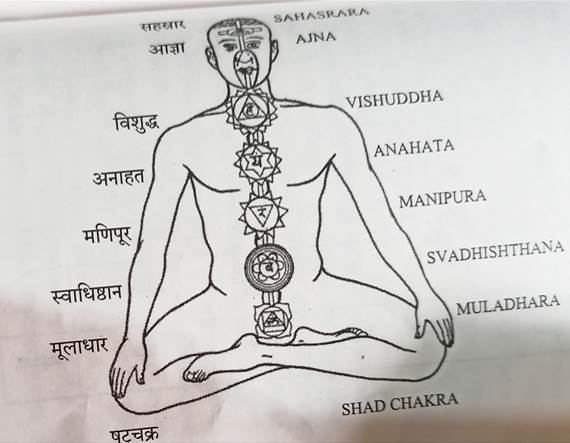
४. स्वास्थ्य और दीर्घायु
जीवन और मृत्यु के रहस्य में अभी भी अनेक बुद्धिमान अन्वेषक जरावस्था और मृत्यु के कारण को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। मानव जीवन कोशिकाओं के पुनरुत्पादन द्वारा चलता है। कोशिकीय द्रव जिसमें नाभिक होता है,, के पुज को कोशिका कहते हैं। मानव शरीर का निर्माण कई प्रकार की कोशिकाओं के अनेक समूहों से हुआ है। ये भिन्न-भिन्न कार्यों का सम्पादन करती हैं और इनका विखंडन और पुनर्निर्माण निरंतर होता रहता है। एक समयावधि के पश्चात् इनकी पुनर्निर्माण क्षमता कम हो जाती है। और अब वह वृद्ध होने लगता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि शरीर का प्रत्येक भाग सात वर्ष में पूर्ण नवीन हो जाता है ।
ऊतक कई प्रकार के होते हैं जैसे—पेशी ऊतक, नाड़ी ऊतक आदि। संस्थान भी कई प्रकार के हैं जैसे—पाचन संस्थान, नाड़ी संस्थान आदि। पाचन संस्थान में मुख, अन्न नलिका, आमाशय, ' छोटी आँत, बड़ी आँत आती है। परिसंचरण संस्थान में हृदय, धमनी तथा कोशिकायें आती हैं। लसिका प्रणाली में लसिका वाहिनी, लसिका ग्रंथियाँ आदि आती हैं।
पेशी संस्थान में जिसमें त्वचा आती है, इसमें बाह्य त्वचा, उप त्वचा, तथा स्वेद ग्रंथियाँ जिनसे पसीना निकलता है तथा त्वगवसीय ग्रंथियाँ जिनसे बसा स्रवित होती है, आती हैं। मूत्र संस्थान में गुर्दे, मूत्राशय तथा मूत्र नलिकार्ये आती हैं। प्रजनन संस्थान में पुरुषों में वृषण, स्त्रियों में गर्भाशय और अण्डाशय आते हैं । अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जैसे गर्दन में अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि तथा अधिवृक्क ग्रंथियाँ । शरीर के ऊतकों में होने वाले उपचय तथा विखंडन के परिवर्तनों के औसत को चयापचय कहते हैं।
एक वैज्ञानिक का विश्वास है कि रक्त परिसंचरण संस्थान में मृत्यु का रहस्य सन्निहित है और इसी कारण वह रासायनिक पदार्थ द्वारा रक्त का उपचार करता है।
एक अन्य वैज्ञानिक का विश्वास है कि जीवन का स्थान अवटु ग्रंथि है। इसलिए वह वृद्ध हो चुकी अवटु ग्रंथियों को चिम्पांजी की युवा वेरिल ग्रंथियों से स्थानांतरित करता है। अन्य वैज्ञानिक सोचते हैं कि वृद्धावस्था मानव शरीर कुछ मुख्य ग्रंथियों के क्षय के कारण होती है। ऐसे कई उदाहरण है कि दुर्बल मनुष्यों को इन ग्रंथियों का रस मुँह के द्वारा अथवा इंजेक्शन के द्वारा देने से वे स्वस्थ भी हो गये। ऐसे चमत्कार नित्य ही होते रहते हैं, लेकिन वे रोगी व्यक्तियों को स्वस्थ मात्र करते हैं। ये जीवन की सामान्य अवधि में वृद्धि नहीं करते और न ही वे चिर-युवा बने रहने में आने वाले प्रतिरोधों का सामना करने में सहायता ही करते हैं। वे एक अस्सी वर्षीय वृद्ध को सौ वर्ष की आयु तक पहुँचाने में सक्षम नहीं हैं। कोशिकाओं के विखंडन की प्रक्रिया जिसे वृद्धावस्था कहते हैं, से मनुष्य आज भी मर रहा है।
रोगी यदि अधेड़ है तो उसके पुनर्नवीनीकरण का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे एक थके हुए व्यक्ति को शराब की बोतल से उत्तेजना आती है और वह शीघ्र ही पुनः गिर पड़ता है। वे नेत्र जिनमें कुछ देर के लिए चमक आयी थी, पुनः निस्तेज हो जाते हैं। मस्तिष्क थोड़ी सी देर के लिए अत्यंत तीव्रता से कार्य करता है और बाद में पुनः कमजोरी अपना प्रभाव दिखाने लगती है। कृत्रिम रूप से उपचारित करके ग्रंथियों को उनकी क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि ये वैज्ञानिक इन कोशिकाओं को जिस प्रकार वे युवावस्था में स्वयं ही अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करती थीं, उसी प्रकार वे वृद्धावस्था में भी प्राप्त कर लें, ऐसी कोई खोज विश्वसनीयता से करते, तो इस मानव शरीर के उपयोग की कोई सीमा नहीं होती। शरीर का सौन्दर्य, शोभा और अभेद्य सुदृढ़ता-ये सभी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ है। • भोजन ऊर्जा का पुंज है। शरीर किसी अन्य स्रोत पर निर्भर हो सकता है--जैसे सूर्य, दिव्य प्राण, संकल्प शक्ति आदि। हठयौगिक क्रियाऐं शरीर में आंतरिक रूप से सुधार करती है तथा कोशिकाओं को नवीन शक्ति, ओज और जीवनी शक्ति प्रदान करती है। योगी ऊर्जा के अवशोषण तथा शरीर के संरक्षण के लिए ऊर्जा के प्रयोग की विधि का ज्ञान रखते हैं। उनके पास अत्यधिक गर्मी और शीत को सहन करने तथा भोजन और जल के बिना जीने की क्षमता होती है। वे इन सभी शक्तियों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त करता है। शरीर को स्वस्थ रखने की एक और विधि है— वायु कुंभक । इस विधि में वायु को निगला या खाया जाता है। इससे शरीर अभेद्य हो जाता है और उसे कोई आघात नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे योगी को रोग, मृत्यु अथवा कष्ट का अनुभव नहीं होता ।
योगी चाँगदेव सौ वर्ष तक जिये। वे आलंदी (महाराष्ट्र) के योगी ज्ञानदेव को देखने के लिए बाघ पर सवार हो कर गये थे। उनके सामने मृत्युदेव यमराज जब भी आते थे तो वे अपने प्राणों को सुषुम्ना में ले कर चले जाते थे और समाधिस्थ हो जाते थे। इस प्रकार उन्होंने कई बार मृत्युदेव को पराजित किया । योगियों के पास इच्छा मृत्यु की सिद्धि होती है।
५. ब्रह्मचर्य द्वारा जीवन में वृद्धि
वीर्य के संरक्षण से पुरुष शरीर की पूर्णता, नवयौवन और दीर्घायु को प्राप्त करता है। यदि पुरुष के शरीर से वीर्य का स्रवण निरंतर होता रहे, तो या तो यह शरीर से निष्कासित हो जाता है अथवा यह अवशोषित हो जाता है। वर्तमान में प्रमाणित तथा निरंतर किये जाने वाले वैज्ञानिक अन्वेषणों के द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि जब वीर्य का संरक्षण किया जाता है, तो यह शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह रक्त का पोषण करता है और मस्तिष्क को बल प्रदान करता है। शरीर को शक्तिशाली तथा मन को ओजस्वी बनाने के लिए और बुद्धि की प्रखरता हेतु वीर्य का संरक्षण आवश्यक है।
वीर्य का नाश चाहे ऐच्छिक हो अथवा अनैच्छिक जीवनी शक्ति का प्रत्यक्ष नाश है । अब तो यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि रक्त के कुछ विशेष घटक वीर्य के संघटन में भाग लेते हैं। यदि ये निष्कर्ष सही हैं तो इनसे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए नैतिकतापूर्ण जीवन बिताना आवश्यक है।
ब्रह्मचर्य काया सिद्धि प्राप्त करने का मुख्य आधार है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास द्वारा वीर्य ओज़ शक्ति में परिणित हो जाता है। ओज़ शक्ति से समस्त कोशिकायें सजीव अथवा विद्युत शक्ति संपन्न हो जाती हैं।
ब्रह्मचर्य के पालन में शीर्षासन, प्राणायाम और ध्यान सहायक होते हैं। ये शरीर को भीतर से पुनर्जीवित करते हैं और कोशिकाओं को नवीन बल, ओज़ और जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। योगी का शरीर निर्दोष होता है। उसके क्रियाकलापों में आकर्षण और शिष्टता होती है। वह इच्छा मृत्यु का स्वामी होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं: "तस्माद्योगी भवार्जुन " — इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो।
यदि योगी काया सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो समस्त रोग और उनकी प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। वह समस्त द्वंदों जैसे सर्दी-गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। मल-मूत्र की मात्रा न्यून हो जाती हैं अथवा ये अदृश्य हो जाते हैं। भूख-प्यास की इच्छा समाप्त हो जाती है। वह भोजन बहुत ही थोड़ा लेता है अथवा भोजन त्याग देता है। उसे किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। सर्दी-गर्मी अथवा दर्द के स्थान पर उसे कुछ सुखदायक अनुभव होते हैं।
अणिमा, महिमा और लधिमा, ये सभी सिद्धियाँ काया सिद्धि के अंतर्गत आती हैं। योगियों और ऋषियों तथा आयुर्वेद की कायाकल्प की विधि को जिससे कि नवयौवन की पुनः प्राप्ति होती है, उसे वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों की पश्चिमी विधि (जिसमें व्यक्ति का उपचार भौतिक आधार पर किया जाता कायाकल्प विधि को पराजित नहीं कर सकती है, क्योंकि कायाकल्प की क्रियाविधि महान् तपस्वियों द्वारा प्रयोग की जा चुकी है तथा इसके द्वारा उन्होंने नवयौवन प्राप्त किया है । कायाकल्प वास्तव में एक आयुर्वर्धक रसायन है जो शरीर को स्थायित्व प्रदान करता है।
इसके द्वारा आप जब तक चाहे अपने शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाये रख सकते हैं। वास्तव में यह शरीर हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधन है । कल्पना करें एक मनुष्य योगाभ्यास करता है, लेकिन निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वह नवीन शरीर प्राप्त करता है और पर्याप्त प्रगति किए बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस प्रकार मरने और पुनः जन्म लेने में बहुत सा समय व्यर्थ चला जाता है । लेकिन यदि हमारा शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली बना रहे, यदि हम जन्म और मृत्यु से मुक्त हो सकें तो हमारे पास योग साधना हेतु बहुत समय होगा और हम अपने जीवन के लक्ष्य को यहीं और इसी जन्म में प्राप्त कर सकेंगे। यही रसायनों का सिद्धान्त है। ये शरीर को अमर बनाना सिखाते हैं, जिससे हम कायाकल्प जिसमें जड़ी-बूटियों, पारा, गंधक अथवा नीम या आँवले का प्रयोग होता है, के द्वारा जीवन के लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त कर सकें ।
इस शरीर का निर्माण मन के द्वारा मन के उपयोग हेतु हुआ है । यह मन ही है जो शरीर का निर्माण करता है। मृत्यु होने पर यह मन इस भौतिक शरीर रूपी आवरण को छोड़ देता है और दूसरे जन्म में नवीन शरीर रूपी आवरण को धारण कर लेता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण-शीर्ण वस्त्र को फेंक कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। मन ऊर्जा के विश्वव्यापी कोष से जितनी चाहे उतनी शक्ति ग्रहण कर सकता है। यदि मन अगले जन्म में नये शरीर का निर्माण कर सकता है, तो वह यही काम बिना इस वर्तमान शरीर को नष्ट किये, उन्हीं कोशिकाओं को नवीन करके जो इस शरीर का निर्माण करती हैं अभी और यहीं क्यों नहीं कर सकता ? यही रसायनों का सिद्धांत है और यही सिद्धांत एकदम सही, ठोस और स्थायी है।
६. धारणा
“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा'"-मन को किसी बाहरी वस्तु अथवा शरीर के भीतर किसी बिन्दु पर केन्द्रित करना धारणा कहलाती है। एक बार संस्कृत के एक विद्वान् ने कबीर से प्रश्न किया—“अभी आप क्या कर रहे हैं?"
कबीर ने उत्तर दिया- “पंडित जी, मैं सांसारिक वस्तुओं से मन हटा कर भगवान के चरण कमलों में लगा रहा हूँ।" इसे ही धारणा कहते हैं। उत्तम चरित्र, आसन, प्राणायाम तथा विषय वस्तुओं से पृथकता धारणा में शीघ्र प्रगति हेतु बड़े ही सहायक हैं। धारणा योग की सीढ़ी का छठवाँ चरण है । मन जहाँ टिक सके, ऐसी किसी वस्तु के बिना धारणा हो ही नहीं सकती । निश्चित उद्देश्य, रुचि तथा एकाग्रता धारणा में सहायक होते हैं।
इन्द्रियाँ आपको बाहर खींच ले जाती हैं तथा आपके मन की शांति को भंग कर देती हैं। यदि आपका मन बेचैन है, तो आप कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते । जब अभ्यास द्वारा मन की किरणें एकत्रित हो जाती हैं, तो मन एकाग्र हो जाता है तथा आपको भीतर से आनंद प्राप्त होता है। उफनते आवेगों को शांत करें ।
आपके भीतर अथक धैर्य, दृढ़ संकल्प तथा सहिष्णुता होने चाहिये। आपको अभ्यास में अत्यधिक नियमित होना चाहिये, अन्यथा आलस्य तथा विरोधी शक्तियाँ आपको लक्ष्य से दूर ले जायेंगी। एक उच्च प्रशिक्षित मन संकल्प के बहिष्कार हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार की धारणा की थोड़ी क्षमता होती है । लेकिन आध्यात्मिक विकास हेतु धारणा का उच्च स्तर तक विकास करना चाहिये। वह थोड़े समय में अधिक कार्य कर सकता है। । धारणा करते समय मस्तिष्क पर कोई तनाव नहीं होना चाहिये । आपको मन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिये ।
वह मनुष्य जिसका मन सभी प्रकार की कल्पनाओं तथा वासनाओं से पूर्ण है, वह किसी भी विषय पर कठिनाई से एक सेकेंड तक ही धारणा कर सकता है । ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, आवश्यकताओं तथा गतिविधियों में कमी, विषय वस्तुओं का त्याग, एकांत वास, मौन का पालन, इंद्रियों का संयम, वासना, लोभ, क्रोध, अनावश्यक लोगों से मिलना-जुलना, समाचार पत्र पढ़ना एवं सिनेमा देखना त्याग दें। इन सभी प्रयत्नों से धारणा शक्ति में वृद्धि होती है ।
सांसारिक दुःखों तथा कष्टों से मुक्ति हेतु एकमात्र उपाय है धारणा । इसके अभ्यासी का उत्तम स्वास्थ्य होता है, वह प्रसन्न रहता है । उसकी अंतर्दृष्टि सूक्ष्म होती है । वह किसी भी कार्य को बड़ी ही दक्षता पूर्वक कर सकता है । धारणा उफनते आवेगों को शुद्ध एवं शांत करती है, विचार शक्ति को दृढ़ करती है एवं योजनाओं को स्पष्ट करती है। यम-नियम द्वारा मन को शुद्ध कीजिये, शुद्धता के बिना धारणा का कोई उपयोग नहीं है।
किसी भी मंत्र का जप एवं प्राणायाम मन को स्थिर करते हैं, विक्षेप दूर करते हैं, धारणा शक्ति में वृद्धि करते हैं। यदि आप सभी विचलनों से मुक्त होंगे तो ही धारणा सम्भव है। जो आपको अच्छा लगे तथा जो मन पसंद करता हो ऐसी किसी वस्तु पर धारणा कीजिये। प्रारंभ में मन को स्थूल विषयों पर धारणा हेतु प्रशिक्षित कीजिये, बाद आप सूक्ष्म वस्तुओं अथवा निर्गुण विचारों पर सफलता पूर्वक धारणा कर सकते हैं। धारणा के अभ्यास में नियमितता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ।
स्थूल विषय : दीवार पर काला बिंदु, मोमबत्ती की लौ, चमकता हुआ तारा, चंद्रमा, ॐ का चित्र, भगवान
राम, कृष्ण, देवी अथवा आपके इष्ट देव के चित्र को अपने सामने रखें। आँखें खुली रखें ।
सूक्ष्म विषय : अपने इष्ट देवता के चित्र के सामने बैठ जाइये । आँखें बंद कर लीजिये । भ्रूमध्य अथवा हृदय
में अपने इष्ट देवता के मानसिक चित्र को लायें। मूलाधार, अनाहत, आज्ञा अथवा अन्य किसी चक्र पर धारणा करें।
७.. यौगिक वर्णमाला
आसन आपको दृढ़ और स्वस्थ बनाते हैं और अनेक रोगों को दूर करते हैं।
भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों का विकास करता है और टी. बी. रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है तथा फेफड़ों की शक्ति तथा क्षमता में वृद्धि करता है।
भुजंग, शलभ और धनुर आसनों के अभ्यास से कब्ज दूर होता है।
धनुरासन भुजंग और शलभ आसनों का संयुक्त रूप है।
संयमित आहार लेना, सादा जीवन और उच्च विचार रखना - ये योगाभ्यासी को उसके लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति में सहायता करते हैं ।
उपवास विष निकालते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं।
गर्भासन पाचन शक्ति तथा भूख में वृद्धि करता है और आँतों के अनेक रोगों को दूर करता है।
हलासन रीढ़ की हड्डी को लचीली बनाता है।
प्रत्याहार और दम के अभ्यास से इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए ।
आसन और प्राणायाम के साथ-साथ ॐ अथवा हरि ॐ का जप भी करना चाहिए ।
कुंभक दीर्घायु प्राप्ति तथा कुंडलिनी जागरण में सहायता करता है ।
लोलासन हाथों और अग्र भुजाओं की माँसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है ।
वैराग्य, अभ्यास, सत्संग, विचार, वासनाओं के उन्मूलन, अहंकार के नाश, प्राणायाम, ध्यान तथा करुणा, सज्जनता, आत्मदमन, शांति और संतोष जैसे सदगुणों के अर्जन के द्वारा मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी शुद्धि प्राप्त होती है ।
ऊर्ध्व पद्मासन स्वप्न दोष को रोकता है, वीर्य शक्ति को ओज शक्ति में रूपांतरित करता है ।
पश्चिमोत्तानासन मोटापा दूर करता है, जठराग्नि बढ़ाता है और पेट के रोगों को दूर करता है।
उपद्रवी इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न उत्तेजना से यदि तुलना की जाये तो क्वेटा का भूकम्प भी कुछ नहीं है।
शीघ्र और ठोस प्रगति के लिए आसन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।
शीर्षासन सब आसनों का राजा है। यह वीर्य शक्ति को ओज शक्ति में रूपांतरित करता है, स्मरण शक्ति तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। और रोगों को दूर करता है ।
त्राटक मन को एकाग्र करने में सहायता करता है और नेत्रों के रोगों को दूर करता है।
उड्डियान बंध उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और जीवनी शक्ति प्रदान करता है। और पाचन संस्थान के रोगों को नष्ट करता है ।
वज्रासन आलस्य को दूर करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पाचन में सहायता करता है और ध्यान हेतु अत्यधिक उपयोगी है।
योग की कठोर साधना हेतु शीत ऋतु श्रेष्ठ समय है।
शीतली और सीत्कारी प्राणायाम के अभ्यास से मुखशुष्कता (मुँह का असामान्य रूप से सूखना) रोग दूर किया जा सकता है।
योग मुद्रा पेट के रोगों को दूर करती है तथा कुंडलिनी का जागरण करती है।
'जीरोसिस' विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। त्राटक तथा शीर्षासन के अभ्यास से यह रोग दूर किया जा सकता है।
८.योग में मूल बंध
अन्नमय कोष जो कि भोजन के सार से बना है उसके पीछे प्राणमय कोष स्थित है जो कि प्राण अथवा प्राण वायु से निर्मित है। यह प्राण शरीर को चलाता है । जब प्राण भौतिक शरीर से अलग हो जाता है, तो जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह सुनिश्चित हो जाती है। यह प्राण संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है ।
प्राण के द्वारा देवता, मनुष्य और पशु जीवित रहते हैं । प्राण ही वास्तव में सभी प्राणियों का जीवन है। इसी कारण इसे वैश्विक जीवन अथवा सभी के लिए जीवन कहा जाता है। जो प्राण की ब्रह्म की भाँति पूजते हैं, वे पूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। यह प्राण सदैव ऊपर-नीचे होता रहता है और मन को अस्थिर रखता है। प्राण के स्पंदन संसार वृक्ष अथवा नश्वर अस्तित्व का कारण हैं ।
योग इस प्राण पर नियंत्रण तथा इस नियंत्रण द्वारा ईश्वर के साथ आनंदपूर्ण ऐक्य प्राप्त करने की विधियों की शिक्षा देता है । प्राणायाम एवं मुद्राओं के अभ्यास से प्राण नियंत्रण में आ जाता है ।
मूल बन्ध एक यौगिक क्रिया है, जो योगाभ्यासी को अपान एवं वीर्य शक्ति को ऊपर ले जाने में सहायता करता है । अपान की नीचे की ओर जाने की प्रवृत्ति है । प्राण और वीर्य शक्ति के इस नीचे की ओर होने वाले प्रवाह को मूल बन्ध के अभ्यास से रोका जाता है। योगाभ्यासी सिद्धासन में बैठ कर अपान और वीर्य शक्ति को गुदा द्वार को संकुचित करके तथा कुंभक के अभ्यास के द्वारा ऊपर की ओर ले कर जाता है । दीर्घकालीन वीर्य शक्ति का नीचे जाने वाला प्रवाह रुकता है और वीर्य ओज़ शक्ति या आध्यात्मिक ऊर्जा में परिणित हो जाता है, यह ध्यान में सहायता करती है ।
यह बंध स्वप्न दोष को रोकता है तथा ब्रह्मचर्य पालन में सहायता करता है । ऐसी लाभदायक यौगिक क्रिया जो प्राचीन काल के ऋषियों और । योगियों द्वारा बतायी गयी, उसका आज लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और वर्तमान काल के कई अनाड़ी अज्ञानी योग साधकों द्वारा इसकी गलत ढंग से व्याख्या की जा रही है। वे इस क्रिया को लोगों को अपने स्वार्थ को साधने के लिए तथा धन कमाने के लिए सिखाते हैं। वे लोगों के समक्ष ऐसा प्रचार करते हैं कि इससे वे अधिक देर तक अपने वीर्य को रोक सकते हैं, जिससे कि वे अधिक देर तक यौन सुख का आनंद ले सकते हैं। वे इस बंध को धनिक लोगों को सिखाते हैं । कुछ भ्रमित गृहस्थ इन दम्भी योगियों (जिनका लक्ष्य सुख-सुविधापूर्ण जीवन हेतु धन कमाना है) के कथनों से मोहित हो जाते हैं और इस क्रिया को सीखने लगते हैं । वे इस क्रिया की शक्ति के कारण इसमें अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं और अपनी जीवनी शक्ति खो बैठते हैं और अल्पकाल में ही चिंता और शरीर का विनाश उन्हें घेर लेता है । इस क्रिया के गलत अभ्यास से अपान अपने स्थान से हट जाती है और उनको तीव्र पेटदर्द, कब्ज़ और बवासीर जैसे अनेक रोग हो जाते हैं ।
इन अनाड़ी योगियों ने लोगों को बड़ी हानि पहुँचाई है । प्राचीन काल के ऋषियों और योगियों की इस उपयोगी क्रिया को ब्रह्मचर्य की प्राप्ति तथा बंध त्रय के रूप में प्राणायाम में सफलता के लिए बताने के स्थान पर, इन भ्रमित आत्माओं ने गृहस्थों को अधिक कामुक बनने हेतु तथा और अधिक कामोपभोग में लिप्त रहने हेतु उत्तेजित किया है। ये योग विज्ञान तथा योगियों पर एक कलंक हैं ।
वे तर्क देते हैं—“हमें आधुनिक युग के अनुसार चलना चाहिए। लोग इसे चाहते हैं । उन्हें इन क्रियाओं से फायदा होगा। वे इस क्रिया के अभ्यास से अधिक सुखी हैं।" वास्तव में क्या ही अद्भुत दर्शन है ? यह विषयासक्त एवं मायावी जनों का दर्शन है। यह विरोचन का दर्शन है। यह माँस का दर्शन है।
हे अज्ञानी मानव ! अपनी आँखें खोलो। अज्ञानता के गहन अंधकार से जागो। ऐसे कपटी योगियों अथवा पाखंडी गुरुओं के मधुर वचनों तथा अश्लील प्रदर्शनों से भ्रमित न हों। ऐसे अभ्यासों को छोड़ दें। वीर्य शक्ति का संरक्षण कीजिए। इसे जप, कीर्तन, प्राणायाम और विचार द्वारा ओज़ शक्ति में परिणित कीजिए । पवित्र जीवन व्यतीत कीजिए। जीवन उच्च उद्देश्यों हेतु बना है।
यह वीर्य आपका बहुमूल्य खज़ाना है । प्रत्येक बूँद का संरक्षण कीजिए। जीवन आत्म साक्षात्कार हेतु निर्मित हुआ है। यहाँ तक कि अब वैज्ञानिक भी खुल कर घोषणा करते हैं कि जिसने वीर्य शक्ति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया है, उसका संपूर्ण शरीर शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से दृढ़ होता है। वह ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करता है, जो कि किसी भी अन्य साधनों से प्राप्त नहीं हो सकती हैं तथा वह अमरता, परम शांति और परमानंद का उपभोग करता है।
हे ज्ञानवान योगी जन, कृपा करके लोगों को गलत राह न दिखायें। स्वयं को प्राचीन काल के पूजनीय ऋषियों का योग्य शिष्य कहें। श्रेष्ठ तथा उदार बनें। ऊँचा लक्ष्य रखें। सच्चे योगी बनें। यदि आप योग के ज्ञान का इस प्रकार प्रचार करेंगे तो विवेकी एवं चरित्रवान जन आप पर हँसेंगे। उन्हें ब्रह्मचर्य पालन के उपायों का ज्ञान प्रदान करें। उन्हें सच्चा योगी बनायें। लोग आपका आदर करेंगे तथा आपकी निष्काम्य सेवा की प्रशंसा करेंगे। यह विश्व ऐसे सच्चे योगियों से पूर्ण हो, जो प्राण, मन तथा वीर्य नियंत्रण हेतु लोगों को सही विधियों की शिक्षा दें। यह भूमि उपरोक्त पाखंडी योगियों से मुक्त हो। सभी उचित बुद्धि एवं योग के सही ज्ञान से युक्त हों। आप सभी पवित्रता एवं दिव्यता का जीवन व्यतीत करें। आप सभी दिव्य योगियों की भाँति चमकें ।
९. नव चक्र विवेक
(सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद के मंत्र )
चक नाम
१. ब्रह्म चक्र ( अधर चक्र )
२. स्वाधिष्ठान चक्र
३. नाभि चक्र
४. मणिपूर चक्र
५. कांता चक्र
६. तालु चक्र
७. भू चक्र
८. आज्ञा अथवा निर्वाण चक्र, ब्रह्मरंध्र का स्थान
९. आकाश चक्र
विवरण :-
१. यह चक्र तीन बार घूमा हुआ है और यह एक देखने में सूर्य के गोले की भाँति है । यहाँ शक्ति अग्नि के
रूप में रहती है। यहाँ कामपीठ है जो कि सभी कामनाओं का दाता है।
२. यहाँ उदयन पीठ है, जो कि व्यक्ति को संसार को अपनी ओर आकृष्ट करने में सहायता करता है।
३. यह सर्प के रूप में पाँच बार कुंडलित है। यहाँ कुंडलिनी का स्थान इतना प्रकाशमान है जैसे कि करोड़ों
सूर्य एक साथ चमक रहे हों और प्रकृति में यह विद्युत की भाँति है ।
४. इस चक्र में कमल की भाँति आठ पंखुड़ियाँ हैं। इसके मध्य में ज्योति का एक बिंदु है।
५. इस चक्र की बाँयीं ओर इडा अथवा चंद्र नाड़ी है तथा इसके दाहिनी ओर पिंगला अथवा सूर्य नाड़ी है।
इसके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, जो कि सफेद रंग की है।
६. यहाँ पर सदा अमृत का प्रवाह होता रहता है। इस बिंदु पर धारणा करने से निर्विकल्प समाधि प्राप्त
होती है।
७. यह चक्र अंगूठे के आकार का है। यहाँ ज्ञान चक्षु स्थित है, जो कि एक बड़े दीपक के समान है।
८. यह परब्रह्म चक्र भी है। यह जालंधर पीठ का स्थान है, जो आनंद अथवा मोक्ष का दाता है।
९. यह सोलह पंखुड़ियों वाले कमल के आकार का है। यहाँ महान् शक्ति है।
१०. यह सभी कामनाओं के अंत को अभिव्यक्त करता है।
तिरुमूलर ने अपने तिरुमतिरम् में निम्न चक्रों के बारे में बताया है, ये इस प्रकार है—तिरुवंबला चक्र, त्रिपुरा चक्र, एरोली चक्र, भैरव चक्र, भुवनपति चक्र और नवाक्षरी चक्र ।
स्वास्थ्य हेतु नासिका से जल पिएँ
नासिका से जल पीने को आयुर्वेद में ऊषापान करना कहते हैं। यह बिस्तर से उठने के तत्काल बाद किया जाता है। इसके लिए जल की मात्रा आठ से पच्चीस औंस होनी चाहिए। इसके लिए जल का तापमान लगभग रक्त के तापमान के बराबर होना चाहिए।
अभ्यासी को थोड़ा आगे की ओर सिर झुका कर खड़े होना चाहिए। इसके बाद उसे एक कप में जल इस प्रकार लेना चाहिए कि नासिका का अग्र भाग जल में डूब जाये। इसके बाद कप को थोड़ा झुकायें और जल को धीरे-धीरे चूसें, उसी प्रकार जैसे लार निगली जाती है। इसे बड़े ही धैर्य पूर्वक एवं आराम से करें। आप आगे बढ़ेंगे। अभ्यास में अच्छी तरह आगे बढ़ने पर अभ्यासी नासिका से जल पी कर मुँह से बाहर निकाल सकता है। वह इसके विपरीत भी कर सकता है। जल को निकालने की एक अन्य विधि है। इसके लिए वह दाहिने नासारंध्र को बंद करके बाँयें नासारंध्र से जल खींचता है और तत्काल बाँयें नासारंध्र को बंद करके दाहिने नासारंध्र से बाहर निकाल देता है। वह इस विधि को कई बार दोहरा सकता है। इसके बाद उसे यही क्रिया विपरीत ओर से करनी चाहिए ।
लाभ
यह क्रिया अत्यंत सरल है, लेकिन इसके बहुत से लाभ हैं। इससे मस्तिष्क और केंद्रीय नाड़ी संस्थान सजीव हो जाते हैं। मस्तिष्क और क्रियाशील तथा तीक्ष्ण हो जाता है। इससे सारे दिन मस्तिष्क ठंढा रहता है। चेहरे की माँसपेशियाँ उत्तेजित हो जाती हैं। धीरे-धीरे चेहरे की झुर्रियाँ अदृश्य हो जाती हैं और मुख पर यौवन आ जाता है। नासिका से जल पीते समय अश्रुग्रंथियाँ अपने स्राव को निकालती हैं। नेत्र इस क्रिया से अच्छी तरह धुल जाते हैं। वे स्पष्ट और चमकीले हो जाते हैं। नेत्रों के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। लंबे समय तक अभ्यास करने से दूर दृष्टि (दूर की चीजें देखने की क्षमता) प्राप्त हो जाती है। नासिका के भीतर का स्थान स्वच्छ रहता है और अभ्यासी कभी भी सर्दी और सिरदर्द से पीड़ित नहीं होता।
प्राणायाम के अभ्यासियों को उनके अभ्यास में लाभ प्राप्त होता है। पित्त की अधिकता से पीड़ित लोगों को भी इससे लाभ होता है। उषापान के उपरांत नौलि क्रिया करने अधिक फायदा होता है । आंतों का प्रबल क्रमाकुंचन सही प्रकार से होने लगता है तथा कब्ज दूर हो जाती है । नासिका की श्लेष्माकला का शोध एवं नाक से अधिक पानी, सर्दी जुकाम तथा नाकिसा के अन्य रोग दूर हो जाते हैं ।
परिशिष्ट
शरीर के संपूर्ण विकास के लिए आसन
अभ्यास क्रम १
१. सिर के बल किए जाने वाले आसन :
शीर्षासन, ऊर्ध्व पद्मासन, सर्वांगासन, वृक्षासन
२. आगे झुकने वाले आसन :
पश्चिमोत्तानासन, हलासन, पादहस्त आसन, योगमुद्रा, महामुद्रा
३. पीछे की ओर झुकने वाले आसन :
धनुरासन, भुजंगासन, चक्रासन, मत्स्यासन, सुप्तवज्रासन
४. रीढ़ मोड़ने वाले आसन :
अर्धमत्स्येंद्रासन
५. पेट के आसन :
मयूरासन, शलभासन, नौलि क्रिया, उड्डियान बंध
६. वक्ष और फेफड़ों के आसन :
भुजंगासन, प्राणायाम
७. बगल की ओर झुकने वाले आसन :
त्रिकोणासन, ताड़ासन
८. शिथिलीकरण : शवासन
अभ्यास क्रम २
|
समूह |
अंग |
आसन |
|
१. |
सिर, मस्तिष्क, कान, नेत्र, नाक |
शीर्षासन, सर्वांगासन, ऊर्ध्वपद्मासन, नेति, कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम |
|
२. |
गर्दन, कंधे |
सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, जालंधर बंध |
|
३. |
धड़, फेफड़े, हृदय |
शलभासन, भुजंगासन, धनुरासन, प्राणायाम |
|
४. |
उदर क्षेत्र, आमाशय, अग्न्याशय, यकृत, आँतें |
पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, धनुरासन, लोलासन, पादहस्तासन, मत्स्येंद्रासन, योगमुद्रा, महामुद्रा, नौलि, उड्डियान बंध |
|
५. |
हाथ, पैर |
त्रिकोणासन, पादहस्तासन, लोलासन, महामुद्रा, मयूरासन, उत्थित पद्मासन |
|
६. |
शिथिलीकरण |
शवासन |
विशेष निर्देश
१. अपने स्वभाव, क्षमता एवं समय की उपलब्धता के अनुसार अभ्यास क्र. १ अथवा २ में से प्रत्येक से
एक अथवा दो आसनों का चुनाव कर लीजिए। यदि आप इन आसनों के लिए कुछ मिनट भी नित्य देंगे तो यह आपके शरीर के संपूर्ण विकास हेतु पर्याप्त होगा। अभ्यास क्रमांक १ तथा २ में आप सभी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। आसनों की प्रविधि को अच्छी तरह समझें, तत्पश्चात् धीरे से उनका अभ्यास प्रारंभ करें। आपको अभ्यास में अत्यधिक नियमित होना चाहिए, तभी आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
२. अभ्यास क्रमांक १ एवं २ में मैंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण आसन दिए है, जिनका अभ्यास सभी सुरक्षित
रूप से कर सकते हैं। पुस्तक में दर्शायी गयी अन्य क्रियाओं का अभ्यास किया जा सकता है। मूर्छा प्राणायाम, खेचरी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा तथा अन्य कठिन बंधों तथा आसनों को गुरु के निर्देशन में किया जाना चाहिए।
३. अपने अभ्यास में नियमित और क्रमबद्ध रहें। जब आप बीमार हों तो अभ्यास रोक दें।
४. जप, धारणा तथा ध्यान हेतु प्रातःकाल ४ बजे से ६ बजे तक का समय श्रेष्ठ है। जैसे ही आप जागें, नींद
भगाने के लिए आप शीर्षासन और थोड़े प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तत्पश्चात् जप तथा ध्यान हेतु बैठ जायें। यदि जप तथा ध्यान के पूर्व प्राणायाम कर लें तो आपकी धारणा गहन होगी। ध्यान के पश्चात् १५ मिनट विश्राम करें, तत्पश्चात् आसनों का अभ्यास आरंभ करें। सर्वप्रथम आसन करें, उसके बाद ताड़न क्रिया, अश्विनी मुद्रा, शक्ति चालन, महा मुद्रा, महा बंध और महा वेध का अभ्यास करें। कंद को एड़ियों से पीटना ताड़न क्रिया का अन्य प्रकार है। आपको अपनी सुविधा तथा समय के अनुसार एक क्रम बना लेना चाहिए ।
५. प्राणायाम के अभ्यास से आप वायु में तैर सकते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, आहार में
संयम रखें और आपकी अच्छी धारणा हो तो कुछ माह तक नियमित प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात् आप हवा में तैर सकेंगे। यह क्रिया गुफा में नहीं की जा सकती है। अभ्यासी का सिर गुफा में टकरा जायेगा । उसे एक विशेष रूप से निर्मित कमरे में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वायु में तैरना मात्र तभी हो सकता है जब नाड़ियाँ शुद्ध हों।
६. प्रारंभ में आपको प्राणायाम की संख्या को गिनना चाहिए और देखना चाहिए कि आप किस प्रकार
विकास कर रहे हैं। उच्च अवस्थाओं में आपको गिनती लगा कर मन को भटकने नहीं देना है। प्राणायाम का अभ्यास तब तक न करें जब तक आप थक न जायें। यौगिक क्रियाओं की समाप्ति के तत्काल बाद न नहायें। आधे घंटे तक विश्राम करें।
७. अभ्यास में शर्म का अनुभव न करें। अभ्यास हेतु उस दिन की प्रतीक्षा न करें जब गुरु आपके पास में
बैठ कर आपको शिक्षा देंगे। यदि आप लगनशील, नियमित और व्यवस्थित हैं और यदि आप इस पुस्तक में दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आश्चर्यजनक प्रगति करेंगे।
बीस महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक नियम
१. ब्राह्ममुहूर्त - जागरण - नित्यप्रति प्रातः चार बजे उठिए। यह ब्राह्ममुहूर्त ईश्वर के ध्यान के लिए बहुत
अनुकूल है।
२. आसन-पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन पर जप तथा ध्यान के लिए आधे घण्टे के लिए पूर्व अथवा
उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। ध्यान के समय को शनैः-शनैः तीन घण्टे तक बढ़ाइए। ब्रह्मचर्य तथा स्वास्थ्य के लिए शीर्षासन अथवा सर्वांगासन कीजिए। हलके शारीरिक व्यायाम (जैसे टहलना आदि) नियमित रूप से कीजिए। बीस बार प्राणायाम कीजिए।
३. जप - अपनी रुचि या प्रकृति के अनुसार किसी भी मन्त्र (जैसे 'ॐ', 'ॐ नमो नारायणाय', 'ॐ नमः
शिवाय', 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय', 'ॐ श्री शरवणभवाय नमः', 'सीताराम', 'श्री राम', 'हरि ॐ' या गायत्री) का १०८ से २१,६०० बार प्रतिदिन जप कीजिए (मालाओं की संख्या १ और २०० के बीच) ।
४. आहार- संयम — शुद्ध सात्त्विक आहार लीजिए। मिर्च, इमली, लहसुन, प्याज, खट्टे पदार्थ, तेल, सरसों
तथा हींग का त्याग कीजिए। मिताहार कीजिए। आवश्यकता से अधिक खा कर पेट पर बोझ न डालिए। वर्ष में एक या दो बार एक पखवाड़े के लिए उस वस्तु का परित्याग कीजिए जिसे मन सबसे अधिक पसन्द करता है। सादा भोजन कीजिए। दूध तथा फल एकाग्रता में सहायक होते हैं। भोजन को जीवन-निर्वाह के लिए औषधि के समान लीजिए। भोग के लिए भोजन करना पाप है। एक माह के लिए नमक तथा चीनी का परित्याग कीजिए। बिना चटनी तथा अचार के केवल चावल, रोटी तथा दाल पर ही निर्वाह करने की क्षमता आपमें होनी चाहिए। दाल के लिए और अधिक नमक तथा चाय, काफी और दूध के लिए और अधिक चीनी न माँगिए।
५. ध्यान- कक्ष — ध्यान-कक्ष अलग होना चाहिए। उसे ताले - कुंजी से बन्द रखिए ।
६. दान—प्रतिमाह अथवा प्रतिदिन यथाशक्ति नियमित रूप से दान दीजिए अथवा एक रुपये में दस पैसे
के हिसाब से दान दीजिए।
७. स्वाध्याय——गीता, रामायण, भागवत, विष्णुसहस्रनाम, आदित्यहृदय, उपनिषद्, योगवासिष्ठ,
बाइबिल, जेन्द-अवस्ता, कुरान आदि का आधा घण्टे तक नित्य स्वाध्याय कीजिए तथा शुद्ध विचार रखिए।
८. ब्रह्मचर्य - बहुत ही सावधानीपूर्वक वीर्य की रक्षा कीजिए। वीर्य विभूति है। वीर्य ही सम्पूर्ण शक्ति है।
वीर्य ही सम्पत्ति है। वीर्य जीवन, विचार तथा बुद्धि का सार है।
९. स्तोत्र पाठ - प्रार्थना के कुछ श्लोकों अथवा स्तोत्रों को याद कर लीजिए। जप अथवा ध्यान आरम्भ
करने से पहले उनका पाठ कीजिए। इसमें मन शीघ्र ही समुन्नत हो जायेगा।
१०. सत्संग—निरन्तर सत्संग कीजिए। कुसंगति, धूम्रपान, मांस, शराब आदि का पूर्णतः त्याग कीजिए।
बुरी आदतों में न फँसिए।
११. व्रत - एकादशी को उपवास कीजिए या केवल दूध तथा फल पर निर्वाह कीजिए।
१२. जप माला-जप-माला को अपने गले में पहनिए अथवा जेब में रखिए। रात्रि में इसे तकिये के नीचे
रखिए।
१३. मौन-- व्रत - नित्यप्रति कुछ घण्टों के लिए मौनव्रत कीजिए।
१४. वाणी-संयम — प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलिए। बोलिए। मधुर बोलिए। थोड़ा
१५. अपरिग्रह — अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए। यदि आपके पास चार कमीजें हैं, तो इनकी
संख्या तीन या दो कर दीजिए। सुखी तथा सन्तुष्ट जीवन बिताइए। अनावश्यक चिन्ताएँ त्यागिए। सादा जीवन व्यतीत कीजिए तथा उच्च विचार रखिए।
१६. हिंसा - परिहार — कभी भी किसी को चोट न पहुँचाइए (अहिंसा परमो धर्मः)। क्रोध को प्रेम, क्षमा तथा
दया से नियन्त्रित कीजिए।
१७. आत्म-निर्भरता — सेवकों पर निर्भर न रहिए। आत्म- निर्भरता सर्वोत्तम गुण है।
१८. आध्यात्मिक डायरी- सोने से पहले दिन भर की अपनी गलतियों पर विचार कीजिए। आत्म-विश्लेषण
कीजिए। दैनिक आध्यात्मिक डायरी तथा आत्म-सुधार रजिस्टर रखिए। भूतकाल की गलतियों का चिन्तन न कीजिए।
१९. कर्तव्य पालन — याद रखिए, मृत्यु हर क्षण आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अपने कर्तव्यों का पालन
करने में न चूकिए। सदाचारी बनिए।
२०. ईश - चिन्तन —– प्रातः उठते ही तथा सोने से पहले ईश्वर का चिन्तन कीजिए। ईश्वर को पूर्ण
आत्मार्पण कीजिए ।
यह समस्त आध्यात्मिक साधनों का सार है।
इससे आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। इन नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन
करना चाहिए। अपने मन को ढील न दीजिए।
-स्वामी शिवानन्द