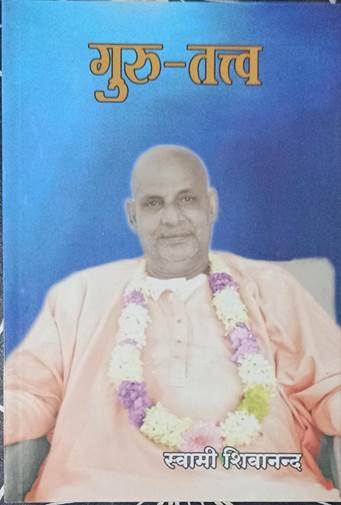
गुरु-तत्त्व
GURU TATTVA का हिन्दी रूपान्तर
लेखक
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती
SERVE LOVE MEDITATE REALIZE
THE DIVINE LIFE SOCIETY
अनुवादक
श्री कामेश्वरस्वरूप गर्ग
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर- 249192
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org.www.dilshq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण- १९८५
षष्ठ हिन्दी संस्करण-२०१८
(१,००० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
ISBN 81-7052-102-5
HS 53
PRICE : ₹55/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए
स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त
फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर, जि. टिहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड, पिन २४९ १९२' में मुद्रित।
For online orders and Catalogue visit: disbooks.org
प्रकाशकीय वक्तव्य
यद्यपि आध्यात्मिक गुरु की धारणा के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा चुका है; फिर भी इस महत्त्वपूर्ण विषय को ले कर जनसाधारण के मन में अनेक भ्रान्तियाँ, भ्रम और सन्देह बने हुए हैं।
क्या साधक के लिए गुरु एक अनिवार्यता है? सद्गुरु कौन है? वह किस सीमा तक अपने शिष्य की सहायता कर सकता है? शिष्य के क्या-क्या कर्तव्य हैं ? दीक्षा का क्या अर्थ है? इनके तथा इनसे सम्बन्धित अनेक प्रश्नों के सुस्पष्ट तथा सुनिश्चित उत्तर उपलब्ध न होने के कारण अनेक उत्साही साधकों की आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है।
आशा है, इन परिस्थितियों में सद्गुरु शिवानन्द जी महाराज की प्रस्तुत पुस्तक अनेक साधकों के लिए वरदान सिद्ध होगी। इस पुस्तक में पाठकों को गुरु-शिष्य के पारस्परिक सम्बन्धों की प्रामाणिक तथा सारगर्भित व्याख्या पढ़ने को मिलेगी।
आध्यात्मिक तृष्णा से आकुल-व्याकुल नर-नारियों के लाभ के लिए इस पुस्तक को प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। भगवान् तथा ब्रह्मविद्या-गुरुओं की कृपा आप सब पर बनी रहे !
यह पुस्तक मूल अँगरेजी पुस्तक Guru-Tattva का अनुवाद है।
-द डिवाइन लाइफ सोसायटी
-
विश्व - प्रार्थना
हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव!
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है।
तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ हो ।
तुम सच्चिदानन्दघन हो ।
तुम सबके अन्तर्वासी हो ।
हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समत्व प्रदान करो।
श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो ।
हमें आध्यात्मिक अन्तःशक्ति का वर दो,
जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों।
हम अहंकार, काम, लोभ, घृणा, क्रोध और द्वेष से रहित हों।
हमारा हृदय दिव्य गुणों से परिपूरित करो ।
हम सब नाम-रूपों में तुम्हारा दर्शन करें।
तुम्हारी अर्चना के ही रूप में इन नाम-रूपों की सेवा करें।
सदा तुम्हारा ही स्मरण करें।
सदा तुम्हारी ही महिमा का गान करें।
तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे अधर-पुट पर हो।
सदा हम तुममें ही निवास करें ।
- स्वामी शिवानन्द
विषय-सूची
शिष्य के कर्तव्य तथा विशेषाधिकार
पावन गुरुपूर्णिमा-दिवस की अर्थवत्ता
महर्षि व्यास तथा हिन्दू-शास्त्रों को उनका योगदान
भगवान् दत्तात्रेय तथा उनके चौबीस गुरु
प्रथम अध्याय
गुरु की भूमिका
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
"उस गुरु को नमस्कार है जो अज्ञान रूपी तिमिर से अन्धे बने लोगों के नेत्र को ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से खोल देता है।"
(गुरुगीता)
गुरु साक्षात् भगवान् है जो साधकों के पथ-प्रदर्शन के लिए साकार रूप में प्रकट होता है। गुरु का दर्शन भगवद्-दर्शन है। गुरु का भगवान् के साथ योग होता है। वह अन्य लोगों में भक्ति अनुप्राणित करता है। उसकी उपस्थिति सबके लिए पावनकारी है।
गुरु वस्तुतः जीवात्मा के मध्य की कड़ी है। गुरु वह सत्ता है जिसने अपने को त्वम् (जीवत्व) से तत् (ब्रह्म) में उन्नत कर लिया है और इस प्रकार उसकी उभय लोकों में मुक्त तथा अबाधित पहुँच है। वह मानो कि अमरत्व की देहली पर खड़ा है और नीचे झुक कर एक हाथ से संघर्षरत आत्माओं को उन्नत करता और दूसरे हाथ से उन्हें नित्य-स्थायी आनन्द तथा असीम सच्चित् की परम सत्ता में ऊपर उठाता है।
सद्गुरु
ग्रन्थों के अध्ययन मात्र से कोई गुरु नहीं बन सकता है। जो श्रोत्रिय हो तथा जिसे आत्मा की अपरोक्षानुभूति हो, उसी पर गुरु का नामारोपण किया जा सकता है। जीवन्मुक्त सन्त वास्तविक गुरु है। वह सद्गुरु है। वह ब्रह्म अथवा परमात्मा से अभिन्न होता है। वह ब्रह्मवित् होता है।
सिद्धियों पर आधिपत्य किसी ऋषि की महत्ता घोषित करने अथवा उसके आत्म-साक्षात्कार की उपलब्धि प्रमाणित करने की कसौटी नहीं है। सद्गुरु चमत्कार अथवा सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता फिरता । वह साधकों को आधिभौतिक पदार्थों की विद्यमानता का निश्चय दिलाने, उन्हें प्रोत्साहन देने तथा उनके हृदय में श्रद्धा निवेशित करने के लिए कभी-कभी उन्हें प्रदर्शित कर सकता है। सद्गुरु असंख्य सिद्धियों से सम्पन्न होता है। वह सभी दिव्य ऐश्वर्यों का स्वामी होता है।
सद्गुरु साक्षात् ब्रह्म है । वह आनन्द, ज्ञान तथा करुणा का सागर है। वह आपकी आत्मा का नेतृत्व करने वाला है। वह सुख का स्रोत है। वह आपके समस्त कष्टों, विषादों तथा बाधाओं को विदूरित करता, आपको सम्यक् दिव्य पथ दर्शाता, आपके अज्ञानावरण को विदीर्ण करता, आपको अमर तथा दिव्य बनाता और आपकी निम्न आसुरी प्रकृति को रूपान्तरित करता है। वह आपको ज्ञान-रज्जु देता और इस संसार सागर में डूबते समय आपको पकड़ता है। उसे मात्र एक मनुष्य ही न समझें। यदि आप उसे मनुष्य समझते हैं, तो आप पशु हैं। अपने गुरु की पूजा करें और श्रद्धापूर्वक उन्हें नमस्कार करें।
गुरु भगवान् है । उसकी वाणी भगवद्-वाणी है। उसे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। उसका सान्निध्य अथवा उसकी संगति भी उन्नयनकारी, प्रेरणादायी तथा भावोत्तेजक है। उसका संग ही आत्म-प्रबोधक है। उसके सान्निध्य में रहना आध्यात्मिक शिक्षा है। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी का अध्ययन करें, आपको गुरु की महत्ता ज्ञात हो जायेगी।
मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है; अतः भगवान् मानव-शरीर के द्वारा शिक्षा देता है। आप अपने गुरु में स्व-कल्पित पूर्णता के मानवीय आदर्श को साकार हुआ पाते हैं। यह वह आदर्श है जिसके अनुरूप आप अपना निर्माण करना चाहते हैं। आपका मन सहज ही यह स्वीकार कर लेगा कि ऐसी महान आत्मा आदर करने तथा श्रद्धा रखने योग्य है।
गुरु मोक्ष का द्वार है । वह इन्द्रियातीत सत्-चित् का द्वार है; किन्तु इस द्वार में साधक को ही प्रवेश करना है। गुरु सहायक है; किन्तु व्यावहारिक साधना का वास्तविक कार्य तो साधक के शिर पर ही है।
गुरु की आवश्यकता
अध्यात्म-पथ पर नवीन साधक को गुरु की आवश्यकता हुआ करती है । एक दीपक को जलाने के लिए आपको एक प्रज्वलित दीपक की आवश्यकता होती है; उसी प्रकार एक प्रबुद्ध आत्मा दूसरी आत्मा को प्रबुद्ध कर सकती है।
कुछ लोग कुछ वर्षों तक स्वतन्त्र रूप से अध्ययन करते हैं। कालान्तर में उन्हें गुरु की आवश्यकता यथार्थतः अनुभव होती है। उन्हें पथ में कुछ बाधाएँ मिलती हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि इन अवरोधों अथवा गतिरोधों को कैसे दूर करें। तब वे गुरु की खोज करना आरम्भ कर देते हैं।
जो व्यक्ति बदरीनाथ जा चुका है, केवल वही आपको वहाँ जाने का मार्ग बतला सकता है। आध्यात्मिक पथ में तो अपना मार्ग ढूँढ़ निकालना आपके लिए और भी कठिन है। मन आपको प्रायः बहकायेगा। गुरु पतन के गर्तों और अवरोधों को दूर कर आपको सन्मार्ग पर ले जायेगा । वह आपको बतलायेगा — “यह मार्ग आपको मोक्ष की ओर ले जायेगा, यह आपको बन्धन की ओर ले जायेगा।” आप जाना तो बदरीनाथ चाहते होंगे; किन्तु इस पथ-प्रदर्शन के अभाव में आप दिल्ली जा पहुँचेंगे।
शास्त्र अरण्य के समान हैं। उनमें अस्पष्ट लेखांश होते हैं। उनमें ऐसे भी लेखांश होते हैं जो प्रतीयमानतः परस्पर विरोधी हैं। उनमें ऐसे भी लेखांश पाये जाते हैं जिनके गूढ़ अर्थ, नानाविध अभिप्राय तथा रहस्यात्मक व्याख्याएँ होती हैं। उनमें प्रतिनिर्देश हैं। आपको गुरु की आवश्यकता है जो आपको ठीक अर्थ समझाये, आपके सन्देहों तथा अस्पष्टताओं को दूर करे और आपके सम्मुख उपदेशों का सार प्रस्तुत करे। प्रत्येक साधक को अध्यात्म-पथ में एक गुरु की अपरिहार्य आवश्यकता होती है। गुरु ही आपके दोषों का पता लगा सकता है। अहंकार का स्वरूप ऐसा है कि आप स्वयं अपने दोषों का पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे व्यक्ति अपनी पीठ नहीं देख सकता है, वैसे ही वह अपनी त्रुटियों को नहीं देख सकता है। अपने दुर्गुणों तथा दोषों के उन्मूलन के लिए उसे एक गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए।
किसी गुरु के पथ-प्रदर्शन में रहने वाला साधक पथ-भ्रष्ट होने से जगत् सुरक्षित रहता है। गुरु के साथ सत्संग आपको भौतिक के सभी प्रलोभनों तथा प्रतिकूल शक्तियों से रक्षा करने का एक कवच तथा दुर्ग है।
जिन लोगों ने किसी गुरु के संरक्षण में रह कर अध्ययन किये बिना ही पूर्णता प्राप्त की हो, उनके उदाहरण गुरु की आवश्यकता के विरुद्ध प्रमाण के रूप में उद्धृत नहीं करने चाहिए; क्योंकि ऐसे महापुरुष आध्यात्मिक जीवन की सामान्य प्रसमता न हो कर उसके अपवाद हुआ करते हैं। आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनका आविर्भाव गत जीवनों में की गयी उम्र सेवा, अध्ययन तथा ध्यान के फल-स्वरूप होता है। वे पहले ही गुरु के अधीन अध्ययन कर चुके होते हैं। वर्तमान जन्म केवल उसके आध्यात्मिक फल का निर्वाह है। अतएव उसके द्वारा गुरु का महत्त्व कम नहीं होता है।
कुछ गुरु अपने साधकों को बहकाते हैं। वे सबसे कहते हैं: "स्वयं ही विचार करें। अपने को किसी गुरु के प्रति समर्पित न करें।" जब व्यक्ति यह कहता है : 'किसी गुरु का अनुसरण न करें', तो उसका अभिप्राय श्रोता का गुरु स्वयं बनने का होता है। ऐसे नकली गुरुओं के पास न जायें। उनके प्रवचनों को न सुनें ।
सभी महापुरुषों के गुरु थे। सभी ऋषियों, मुनियों, पैगम्बरों, जगद्गुरुओं, अवतारों, महापुरुषों के; चाहे वे कितने ही महान् क्यों न रहे हों; अपने निजी गुरु थे । श्वेतकेतु ने उद्दालक से, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से, भृगु ने वरुण से, नारद ने सनत्कुमार से, नचिकेता ने यम से, इन्द्र ने प्रजापति से सत्य के स्वरूप की शिक्षा प्राप्त की तथा अन्य अनेक लोग ज्ञानी जनों के पास विनम्रतापूर्वक गये, ब्रह्मचर्य व्रत का अति-नियमनिष्ठा से पालन किया, कठोर अनुशासनों की साधना की तथा उनसे ब्रह्मविद्या सीखी।
भगवान् कृष्ण अपने गुरु सान्दीपनि के चरणों में बैठे। भगवान् राम के गुरु वसिष्ठ थे जिन्होंने उन्हें उपदेश दिया। प्रभु यीशु ने जान से जार्डन नदी के तट पर दीक्षित होने के लिए उन्हें खोजा था। देवताओं के भी बृहस्पति गुरु हैं। दिव्य आत्माओं में से सर्वाधिक महान् भी गुरु दक्षिणामूर्ति के चरणों में बैठे थे।
नव-दीक्षित के लिए प्रथम दैहिक गुरु होना आवश्यक है। वह प्रारम्भ में ही भगवान् को गुरु नहीं बना सकता है। उसका चित्त शुद्ध होना चाहिए। उसमें नैतिक पूर्णता होनी चाहिए। उसे पूर्णरूपेण धार्मिक होना चाहिए। तभी वह भगवान् को अपना गुरु बना सकता है।
गुरु का चयन
यदि आप किसी महात्मा के सान्निध्य में शान्ति पाते हैं; यदि आप किसी के प्रवचनों से अनुप्राणित होते हैं; यदि वह आपकी शंकाओं का समाधान कर सकता है; यदि वह काम, क्रोध तथा लोभ से मुक्त है; यदि वह निःस्वार्थ, स्नेही तथा अस्मिता-रहित है, तो आप उसे अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं। जो आपके सन्देहों का निवारण कर सकता है, जो आपकी साधना में सहानुभूतिशील है, जो आपकी आस्था में बाधा नहीं डालता, वरन् जहाँ आप हैं वहाँ से आगे आपकी सहायता करता है, जिसकी उपस्थिति में आप आध्यात्मिक रूप से अपने को उत्थित अनुभव करते हैं, वह आपका गुरु है। यदि आपने एक बार गुरु का चयन कर लिया, तो निर्विवाद रूप से उनका अनुसरण करें। भगवान् गुरु के माध्यम से आपका पथ-प्रदर्शन करेगा।
अपने गुरु के चयन में अपनी बुद्धि का उपयोग अधिक न करें। ऐसा करने पर आप असफल रहेंगे। यदि आप श्रेष्ठ गुरु प्राप्त करने में असफल हों तो उस साधु की शिक्षाओं का पालन कीजिए जो कुछ वर्षों से उस पथ पर चल रहा हो, जिसमें शुचिता तथा अन्य सद्गुण हों, जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो। जैसे स्नातकोत्तर उपाधि वाले प्राध्यापक के उपलब्ध न होने पर माध्यमिक कक्षा का छात्र तृतीय कक्षा के छात्र को पढ़ा सकता है, जैसे जानपद शल्य-चिकित्सक (सिविलसर्जन) के उपलब्ध न होने पर उपसहायक शल्य-चिकित्सक रोगी का उपचार कर सकता है, वैसे ही यह मध्यम कोटि का गुरु आपकी सहायता कर सकता है।
यदि आप इस मध्यम कोटि के गुरु को पाने में भी असमर्थ हैं, तो आप श्री शंकराचार्य, दत्तात्रेय जैसे आत्मसाक्षात्कार प्राप्त सन्तों द्वारा लिखित ग्रन्थों में अन्तर्विष्ट उपदेशों का अनुसरण कर सकते हैं। यदि प्राप्य हो तो ऐसे साक्षात्कार प्राप्त गुरु का चित्र रख सकते हैं तथा उसकी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पूजा कर सकते हैं। शनैः-शनैः आपको प्रेरणा मिलेगी तथा गुरु स्वप्न में प्रकट होंगे और उचित समय आने पर आपको दीक्षा तथा प्रेरणा देंगे। सच्चे साधक के लिए रहस्यमय ढंग से सहायता आती है।
भगवान् से रहस्यमयी सहायता
जरा देखें कि निम्नांकित उदाहरणों में भगवान् ने भक्त की किस प्रकार सहायता की। एकनाथ ने आकाशवाणी सुनी। उसने कहा- "जनार्दन पन्त से देवगिरि में मिलो। वह तुम्हें ठीक मार्ग में ले जायेंगे तथा तुम्हारा पथ-प्रदर्शन करेंगे।” उन्होंने तदनुसार कार्य किया तथा उन्हें अपना गुरु मिल गया। तुकाराम को अपना मन्त्र 'राम कृष्ण हरि' स्वप्न में मिला। उन्होंने इस मन्त्र का जप किया तथा भगवान् कृष्ण के दर्शन किये। भगवान् कृष्ण ने नामदेव को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मल्लिकार्जुन के एक संन्यासी के पास भेजा। रानी चुडाला ने कुम्भ मुनि का रूप धारण किया, वन में अपने पति शिखिध्वज के सम्मुख प्रकट हुई तथा उन्हें कैवल्य के गूढ़ तत्त्व में दीक्षित किया। मधुर कवि आकाश में लगातार तीन दिन तक ज्योति देखते रहे। इसने उनका मार्ग-प्रदर्शन किया और उन्हें तिन्नेवेली के निकट एक इमली के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ उनके गुरु नम्माल्वर के पास पहुँचाया। बिल्वमंगल चिन्तामणि नर्तकी से बहुत आसक्त थे । पश्चादुक्त उनकी गुरु बनी। तुलसीदास को एक अदृश्य आत्मा से हनुमान् के और हनुमान् के द्वारा श्री राम के दर्शन का अनुदेश प्राप्त हुआ ।
अधिकारी शिष्यों को सुयोग्य गुरु का कभी भी अभाव नहीं रहता है। साक्षात्कार प्राप्त आत्माएँ दुर्लभ नहीं हैं। सामान्य निर्बुद्धि व्यक्ति उन्हें सहजता से पहचान नहीं पाते हैं। कुछ इने-गिने व्यक्ति ही, जो अनघ तथा सद्गुणों के मूर्त रूप हैं, आत्मसाक्षात्कार प्राप्त आत्माओं को पहचान सकते हैं तथा वे ही उनके सान्निध्य से लाभान्वित होते हैं।
जब तक संसार है, तब तक आत्म-साक्षात्कार के पथ में संघर्षरत आत्माओं का पथ-प्रदर्शन करने के लिए गुरु तथा वेद हैं। हो सकता है कि सत्ययुग की अपेक्षा कलियुग में साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं की संख्या अल्प हो; किन्तु साधकों की सहायता करने के लिए वे सदा विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता, प्रकृति तथा बुद्धि के अनुसार अपना मार्ग अपनाना चाहिए। उसके सद्गुरु उस मार्ग में उसे मिलेंगे।
शिक्षा-गुरु तथा दीक्षा-गुरु
इस भूलोक में व्यक्ति के द्विधा कर्तव्य हैं—अपने जीवन का परिरक्षण तथा आत्म-साक्षात्कार। अपने जीवन के परिरक्षण के लिए उसे अपनी दैनिक जीविका हेतु कार्य करना सीखना होता है। आत्म-साक्षात्कार के लिए उसे सेवा, प्रेम तथा ध्यान करना होता है। जो गुरु उसे सांसारिक कलाओं का ज्ञान प्रदान करता है, वह शिक्षा-गुरु है। जो गुरु उसे आत्म-साक्षात्कार का मार्ग प्रदर्शित करता है, वह दीक्षा गुरु है। शिक्षा-गुरु अनेक हो सकते हैं—जितनी बातें वह सीखना चाहता है, उतने गुरु हो सकते हैं। दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है-वही होता है, जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है।
एक गुरु से संलग्न रहें
एक चिकित्सक से आपको औषधि-निर्देश (नुस्खा) मिलता है, दो चिकित्सकों से आपको परामर्श प्राप्त होता है और यदि तीन चिकित्सक हुए, तो आपका अपना दाह-संस्कार होता है। इसी भाँति यदि आपके अनेक गुरु होंगे, तो आप किंकर्तव्यविमूढ़ हो जायेंगे। क्या करणीय है, यह आपको ज्ञात न होगा। एक गुरु आपसे कहेगा, 'सोऽहं का जप करो।' दूसरा आपसे कहेगा, 'श्री राम का जप करो।' तृतीय गुरु आपसे कहेगा, 'अनाहत नाद को सुनो।' आप उलझन में पड़ जायेंगे। एक गुरु से संलन रहें और उनके उपदेशों का पालन करें।
सबकी बातें सुनें; किन्तु अनुगमन एक ही व्यक्ति का करें। सबका सम्मान करें; किन्तु श्रद्धा एक ही व्यक्ति पर रखें। सबसे ज्ञान एकत्र करें; किन्तु एक ही शिक्षक के उपदेशों को अपनायें। तब आपकी आध्यात्मिक प्रगति शीघ्र होगी।
गुरु-परम्परा
आध्यात्मिक ज्ञान गुरु-परम्परा का विषय है। यह गुरु से अपने शिष्य को प्रदान किया जाता है। गौडपादाचार्य ने अपने शिष्य गोविन्दाचार्य को, गोविन्दाचार्य ने अपने शिष्य शंकराचार्य को और शंकराचार्य ने अपने शिष्य सुरेश्वराचार्य को आत्मज्ञान प्रदान किया। मत्स्येन्द्रनाथ ने अपने शिष्य गोरखनाथ को, गोरखनाथ ने निवृत्तिनाथ को और निवृत्तिनाथ ने ज्ञानदेव को ज्ञान प्रदान किया। तोतापुरी ने श्री रामकृष्ण को और रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानन्द को ज्ञान प्रदान किया। राजा जनक के जीवन को ढालने वाले अष्टावक्र थे। राजा भर्तृहरि की आध्यात्मिक नियति को आकार देने वाले गोरखनाथ थे। जब अर्जुन तथा उद्धव के मन अनिश्चित अवस्था में थे, तब भगवान् श्री कृष्ण ने ही उन्हें आध्यात्मिक पथ पर प्रतिष्ठित किया था।
दीक्षा - इसका अर्थ
भक्त सन्त एक भक्त को भक्ति-मार्ग में दीक्षित करता है। ज्ञानी वेदान्त के साधक को महावाक्यों की दीक्षा देता है। हठयोगी तथा राजयोगी अपने-अपने विशेष मार्ग में दूसरों को दीक्षित करते हैं; किन्तु पूर्ण ज्ञानी अथवा पूर्ण योगी किसी भी विशेष मार्ग की दीक्षा दे सकता है। श्री शंकर अथवा मधुसूदन सरस्वती जैसा सन्त अथवा ज्ञानी जिस मार्ग के लिए साधक उपयुक्त है, उसकी उसे दीक्षा दे सकता है। गुरु साधक की सूक्ष्म जाँच द्वारा उसकी अभिरुचि, प्रकृति तथा क्षमता का पता लगा लेता है और उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग निश्चित करता है। यदि उसका हृदय अपवित्र है, तो गुरु उसके लिए कई वर्षों तक निःस्वार्थ सेवा निर्धारित करता है। तब गुरु पता लगाता है कि साधक किस विशेष मार्ग के उपयुक्त है और उसको उसकी दीक्षा देता है।
दीक्षा का अर्थ दूसरे व्यक्ति के कानों में मन्त्रोच्चारण करना नहीं है। यदि राम कृष्ण के विचारों से प्रभावित है, तो राम ने पहले ही कृष्ण से दीक्षा ले ली है। यदि एक साधक एक सन्त द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन करके सन्मार्ग पर चलता है और उसके उपदेशों को आत्मसात् करता है, तो वह सन्त उसका गुरु बन चुका है।
शक्ति-संचार
आप जिस प्रकार एक सन्तरे को एक व्यक्ति को दे सकते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में संचारित कर सकता है। आध्यात्मिक शक्ति को सम्प्रेषित करने की इस विधि को शक्ति-संचार कहा जाता है। शक्ति-संचार में सद्गुरु के कुछ आध्यात्मिक स्फुरण वस्तुतः शिष्य के मस्तिष्क में स्थानान्तरित किये जाते हैं।
गुरु उस उपयुक्त शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है जिसे वह इसके लिए योग्य समझता है। गुरु शिष्य को दृष्टि-निक्षेप, स्पर्श, विचार, शब्द अथवा इच्छा-शक्ति से रूपान्तरित कर सकता है।
शक्ति-संचार परम्परागत है। यह एक गुप्त रहस्यमय विज्ञान है जो गुरु से शिष्य को प्रदान किया जाता है।
प्रभु यीशु ने स्पर्श द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने कुछ शिष्यों में संचारित की। समर्थ रामदास के एक शिष्य ने नर्तकी की उस पुत्री में अपनी शक्ति संचारित की जो उसके प्रति अत्यधिक कामातुर थी। शिष्य ने उसकी ओर एक टक देखा और उसे समाधिस्थ कर दिया। उसकी काम वासना नष्ट हो गयी। वह बहुत ही धार्मिक तथा आध्यात्मिक बन गयी। भगवान् कृष्ण ने अन्धे सूरदास के नेत्रों को स्पर्श किया, सूरदास की अन्तर्दृष्टि खुल गयी। उन्हें भावसमाधि हुई। गौरांग महाप्रभु ने अपने स्पर्श द्वारा अनेक लोगों में दिव्योन्माद उत्पन्न किया और उनका मन अपनी ओर परिवर्तित कर लिया। उनके स्पर्श से नास्तिक आनन्दातिरेक से गलियों में नृत्य तथा हरि-कीर्तन करते थे ।
शिष्य को गुरु के शक्ति-संचार से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे और अधिक पूर्णता तथा उपलब्धियों के लिए साधना में कठोर संघर्ष करना होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानन्द को स्पर्श किया, स्वामी विवेकानन्द को समाधि लग गयी। उन्होंने स्पर्श के बाद भी पूर्णता की प्राप्ति के लिए और सात वर्ष तक कठोर साधना की।
कृपा तथा स्व-प्रयास
आपके गुरु के चमत्कार के फल-स्वरूप आपको आत्म-साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवान् बुद्ध, प्रभु यीशु, रामतीर्थ —सभी ने साधना की थी। भगवान् कृष्ण अर्जुन को वैराग्य तथा अभ्यास विकसित करने के लिए कहते हैं। उन्होंने अर्जुन से यह नहीं कहा : "मैं तुम्हें अभी मुक्ति दे दूँगा।" अतः इस असत् धारणा का परित्याग कर दें कि आपके गुरु आपको समाधि तथा मुक्ति दे देंगे। प्रयास करें, शुद्ध बनें, ध्यान करें तथा आत्म-साक्षात्कार करें ।
गुरु कृपा परमावश्यक है; किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि शिष्य हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहे। उसे कठोर पुरुषार्थ करना होता है। सारा कार्य शिष्य को करना होता है। आजकल तो लोग यह चाहते हैं कि वे संन्यासी के कमण्डल से एक बूँद जल लें और उन्हें तुरन्त समाधि लग जाये। वे निर्मलीकरण तथा आत्म-साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की साधना करने को तैयार नहीं हैं। वे जादू की गोली चाहते हैं जो उन्हें समाधि में धकेल दें। यदि आपको ऐसी भ्रान्ति है, तो उसे तत्काल त्याग दीजिए।
गुरु तथा शास्त्र आपका मार्ग-प्रदर्शन कर सकते हैं और आपके सन्देहों का निवारण कर सकते हैं। अपरोक्षानुभूति तो आपको स्वयं ही करनी होगी। क्षुधित व्यक्ति को स्वयं ही भोजन करना होगा। जिसे दुःसह खुजली हो, उसे स्वयं खुजलाना होगा।
निःसन्देह गुरु का आशीर्वाद सब-कुछ कर सकता है; परन्तु किसी को उसका आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो ? गुरु को प्रसन्न करके ही यह प्राप्त किया जा सकता है। गुरु अपने शिष्य से तभी प्रसन्न होता है, जब उत्तरोक्त उसकी आध्यात्मिक शिक्षाओं का निर्विवाद पालन करता है। अतएव गुरु की शिक्षाओं का सावधानीपूर्वक अनुसरण करें। उसकी शिक्षाओं को कार्यान्वित करें। तभी आप उसके आशीर्वाद के पात्र होंगे और तभी उसका आशीर्वाद सब-कुछ कर सकेगा ।
द्वितीय अध्याय
शिष्य के कर्तव्य तथा विशेषाधिकार
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥
"जिस साधक की परम देव परमात्मा में परम भक्ति हैं तथा (जिसकी भक्ति) जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं।"
(श्वेताश्वतर उपनिषद् : ६-२३)
शिष्य वह है जो गुरु के उपदेशों का अक्षरशः तथा भावशः पालन करता और उनकी शिक्षाओं का प्रचार तथा प्रसार अपने से कम विकसित आत्माओं में आजीवन करता रहता है।
वास्तविक शिष्य केवल गुरु के दिव्य स्वरूप से ही सम्बन्ध रखता है। गुरु जो मानव होने के नाते कार्य करता है, उसकी वह चिन्ता नहीं करता। वह इस ओर पूर्ण विस्मरणशील-सा रहता है। उसके लिए गुरु-गुरु है भले ही वह लोकाचार के विपरीत व्यवहार करे। वह सदा स्मरण रखे कि सन्त का स्वरूप अतलस्पर्श होता है। उनके विषय में अपना कोई मत न बनाइए। अपनी अज्ञानता के अक्षम मापदण्ड से उसके दिव्य स्वरूप को न मापिए । व्यापक दृष्टिकोण से सम्पादित अपने गुरु के कार्यों की आलोचना न कीजिए।
विशुद्ध शिष्यत्व दृष्टि का उन्मीलन करता है। यह आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करता है। यह प्रसुप्त क्षमताओं को उद्बोधित करता है। यह आध्यात्मिक पथ की यात्रा में सर्वाधिक आवश्यक पाथेय है। गुरु तथा शिष्य एक बन जाते हैं। गुरु शिष्य को आशीर्वाद देता, उसका पथ-प्रदर्शन करता तथा उसे प्रेरणा देता है। वह उसमें शक्ति-संचार करता है, उसे रूपान्तरित करता तथा आध्यात्मिक बनाता है।
गुरु का सान्निध्य प्राप्त करने का अधिकारी कौन है
गुरु का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए आपको उपयुक्त अधिकारी होना चाहिए। विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, गुरु में श्रद्धा, भगवद्-भक्ति—इन आवश्यक उपकरणों से सन्नद्ध हो कर साधक को गुरु के समीप जाना चाहिए।
गुरु केवल उसी साधक को आध्यात्मिक उपदेश प्रदान करता है जो मुमुक्षु हो, जो शास्त्रों के आदेशों का यथावत् पालन करता हो, जिसने अपनी दुर्वासनाओं तथा इन्द्रियों का दमन किया हो, जिसका मन शान्त हो तथा जो करुणा, विश्व-प्रेम, धैर्य, विनम्रता, तितिक्षा, सहिष्णुता आदि सद्गुणों से सम्पन्न हो । ब्रह्म के रहस्य की दीक्षा तभी फलित होती है और शिष्य के मन में ज्ञान उत्पन्न करती है, जब शिष्य का मन निष्काम बन जाता है।
गुरु-सेवा
अभीप्सुओं को आरम्भ में अपना सम्पूर्ण अवधान गुरु की दीर्घकालिक सेवा द्वारा स्वार्थपरता के निष्कासन में निर्दिष्ट करना चाहिए। अपने गुरु की सेवा दिव्य भाव से कीजिए। इससे पार्थक्य-रूपी कर्कटार्बुद (कैंसर) विलीन हो जायेगा।
पोत का कप्तान सदा सतर्क रहता है। एक धीवर सदा सतर्क रहता है। शल्य-चिकित्सक शल्यकर्म गृह में सदा सतर्क रहता है। इसी प्रकार पिपासु तथा क्षुधित शिष्य को अपने गुरु की सेवा में सदा सतर्क रहना चाहिए।
गुरु के सेवार्थ जीवन यापन करें। आपको अवसरों की ताक में रहना चाहिए। आमन्त्रण की प्रतीक्षा न कीजिए। गुरु-सेवा के लिए अपने को स्वेच्छा से अर्पित कीजिए ।
अपने गुरु की सेवा नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, निर्विवाद, निरभिमानपूर्वक, खुशी से, अथक रूप से तथा प्रेमपूर्वक कीजिए। आप अपने गुरु की सेवा में जितनी अधिक शक्ति व्यय करेंगे, उतनी ही अधिक दिव्य शक्ति आपमें प्रवाहित होगी।
जो गुरु की सेवा करता है, वह सम्पूर्ण विश्व की सेवा करता है। गुरु की सेवा बिना किसी स्वार्थपरायण उद्देश्य से करें। गुरु की सेवा करते समय अपने आन्तरिक उद्देश्य की संवीक्षा करें। गुरु की सेवा नाम, यश, सत्ता, धन आदि की प्रत्याशा के बिना की जानी चाहिए।
गुरु की आज्ञाकारिता
गुरु के प्रति श्रद्धा रखने की अपेक्षा उनकी आज्ञाओं का पालन करना श्रेष्ठतर है। आज्ञाकारिता एक मूल्यवान् सद्गुण है; क्योंकि यदि आप आज्ञाकारिता के गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे, तो आत्म-साक्षात्कार के पथ के कट्टर शत्रु अहं का शनैः-शनैः उन्मूलन हो जायेगा ।
जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है, केवल वही अपनी निम्न आत्मा पर आधिपत्य रख सकता है। आज्ञाकारिता अत्यन्त व्यावहारिक, अनन्य तथा सक्रिय अध्यवसायी होनी चाहिए। गुरु की आज्ञाकारिता न तो टाल-मटोल करती है और न सन्देह ही प्रकट करती है। दम्भी शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन भयवश करता है। सच्चा शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन प्रेम के लिए प्रेम के कारण करता है।
आज्ञा-पालन की विधि सीखिए। उस स्थिति में ही आप आदेश दे सकते हैं। शिष्य बनना सीखिए, तभी आप गुरु बन सकेंगे।
इस भ्रामक धारणा को त्याग दीजिए कि गुरु की अधीनता स्वीकार करना, उनका आज्ञानुवर्ती होना तथा उनकी शिक्षाओं को कार्यान्वित करना दासता की मनोवृत्ति है। अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि किसी अन्य व्यक्ति की अधीनता स्वीकार करना उसकी गरिमा के प्रतिकूल तथा उसकी स्वाधीनता के विपरीत है। यह एक बड़ी गम्भीर भूल है। यदि आप ध्यानपूर्वक चिन्तन करें, तो आप देखेंगे कि आपकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता वास्तव में आपके अपने ही अहं तथा मिथ्याभिमान की नितान्त घृणित दासता है, यह विषयी मन की तरंग है। जो अपने अहं तथा मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वास्तव में वही स्वतन्त्र व्यक्ति है। वह शूरवीर है। इस विजय को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति गुरु के उच्चतर अध्यात्मीकृत व्यक्तित्व की अधीनता स्वीकार करता है। वह इस अधीनता स्वीकरण द्वारा अपने निम्न अहं को पराजित करता तथा असीम चेतना के आनन्द को प्राप्त करता है।
निश्चिन्त शिष्य
आध्यात्मिक पथ कला की स्नातकोत्तर उपाधि के लिए शोध-प्रबन्ध लिखने जैसा नहीं है। यह सर्वथा भिन्न प्रणाली है। इसमें गुरु की सहायता की आवश्यकता प्रति क्षण रहती है। इन दिनों साधक आत्म-निर्भर, उद्धत तथा स्वाग्रही बन गये हैं। वे गुरु की आज्ञाओं को कार्यान्वित करने की चिन्ता नहीं करते। वे गुरु बनाना नहीं चाहते। वे प्रारम्भ से ही स्वतन्त्रता चाहते हैं। वे समझते हैं कि वे तुरीय अवस्था में हैं, जब कि उन्हें आध्यात्मिकता अथवा सत् का प्रारम्भिक ज्ञान भी नहीं होता। वे स्वेच्छाचारिता अथवा अपनी बात मनवाने और स्वेच्छानुसार चलने को स्वतन्त्रता समझने की भूल करते हैं। यह गम्भीर शोचनीय भूल है। यही कारण है कि उनकी उन्नति नहीं होती। वे साधना की क्षमता तथा ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास खो बैठते हैं। वे कश्मीर से गंगोत्तरी तक और गंगोत्तरी से रामेश्वरम् तक मार्ग में 'विचार-सागर' और 'पंचदशी' से कुछ अनाप-शनाप बकते तथा जीवन्मुक्त होने का ढोंग रचते लापरवाही से निरुद्देश्य ठोकरें खाते फिरते हैं।
समर्पण तथा कृपा
यदि आप नल से जल पीना चाहते हैं, तो आपको अपने को झुकाना पड़ेगा। इसी भाँति यदि आप गुरु के पवित्र ओष्ठों से प्रवाहित होने वाली अमरत्वप्रदायक आध्यात्मिक सुधा का पान करना चाहते हैं, तो आपको विनीतता तथा विनम्रता का मूर्त रूप बनना होगा।
मन की निम्न प्रकृति का पूर्णतया नवीकरण करना चाहिए। साधक अपने गुरु से कहता है 'मैं योगाभ्यास करना चाहता हूँ। ''मैं निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। मैंने आपको आत्म-समर्पण कर दिया है।" परन्तु वह अपनी निम्न प्रकृति और स्वभाव को; पुराने चरित्र, व्यवहार और आचरण को परिवर्तित करना नहीं चाहता।
व्यक्ति को अपने वैयक्तिक अहं, पूर्वावधारित धारणाओं, प्रिय विचारों, पूर्वाग्रहों तथा स्वार्थमयी अभिरुचियों को त्याग देना चाहिए। ये सब गुरु के आदेशों और उपदेशों के कार्यान्वयन में बाधक हैं। अपने हृदय के भेद को अपने गुरु के सम्मुख अनावृत कर दें। आप जितना ही अधिक ऐसा करेंगे, उतनी ही सहानुभूति अर्थात् पाप तथा प्रलोभन के विरुद्ध संघर्ष में आपको शक्ति की प्राप्ति होगी।
गुरु की कृपा की आकांक्षा करने से पूर्व साधक को उसका पात्र बनना चाहिए। दिव्य कृपा की आपूर्ति तभी होती है, जब साधक में सच्ची पिपासा हो और जब वह उसे ग्रहण करने योग्य हो।
गुरु की कृपा उन्हीं पर अवतरित होती है, जो उसके प्रति पूर्णरूपेण विनम्र तथा निष्ठावान् अनुभव करते हैं। निष्ठा गुरु में विश्वास तथा सम्प्रत्यय है। गुरु साक्ष्य अथवा प्राधिकार के रूप में जो घोषित करता है, उसकी सत्यता पर बिना किसी अन्य साक्ष्य अथवा प्रमाण के दृढ़ विश्वास करना निष्ठा है। जिस शिष्य की गुरु में निष्ठा है, वह वाद-विवाद नहीं करता, सोच-विचार नहीं करता, तर्क-वितर्क नहीं करता तथा चिन्तन नहीं करता । वह उसकी आज्ञाओं का मात्र पालन करता है।
शिष्य का गुरु के प्रति आत्म-समर्पण तथा गुरु की कृपा में पारस्परिक सम्बन्ध है। समर्पण गुरु की कृपा को नीचे की ओर आकर्षित करता है और गुरु-कृपा समर्पण को पूर्ण बनाती है। गुरु-कृपा साधक में साधना के रूप में कार्य करती है। यदि साधक अपने पथ में दृढ़तापूर्वक संलग्न रहता है, तो यह गुरु-कृपा है। यदि प्रलोभन के अभ्याक्रमण करने पर वह प्रतिरोध करता है, तो यह गुरु कृपा है। यदि लोग प्रेम तथा सम्मान के साथ उसका स्वागत करते हैं, तो यह गुरु कृपा है। यदि उसे सम्पूर्ण शारीरिक आवश्यकताएँ सुलभ हैं, तो यह गुरु-कृपा है। यदि नैराश्य तथा अवसाद के समय उसे प्रोत्साहन तथा बल प्राप्त होता है, तो यह गुरु-कृपा है। यदि वह शरीर चेतना का अतिक्रमण कर जाता है और अपने आनन्द-स्वरूप में विश्राम करता है, तो यह गुरु कृपा है। प्रत्येक पग पर उसकी कृपा का अनुभव कीजिए तथा उसके प्रति निष्कपट तथा सत्यनिष्ठ रहिए।
गुरु की उपदेश-विधि
गुरु वैयक्तिक उदाहरण द्वारा शिक्षा देता है। गुरु का दैनन्दिन आचरण सतर्क शिष्य के लिए एक जीवन्त आदर्श है। सच्चे शिष्य के लिए गुरु का जीवन एक जीवन्त धर्मोपदेश है। शिष्य अपने गुरु के निरन्तर सम्पर्क द्वारा उसके सद्गुणों को आत्मसात् करता है। वह शनैः-शनैः नव-आकार लेता है। छान्दोग्योपनिषद् को पढ़िए। उसमें आप पायेंगे कि इन्द्र प्रजापति के पास एक सौ एक वर्ष तक रहे और उनकी अनन्य भाव से सेवा की।
अपने शिष्यों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को केवल गुरु ही जानता है। वह शिष्य की प्रकृति तथा विकास के अनुसार उपदेश देता है। इस उपदेश को गुप्त रखना चाहिए। शिष्यों में उसकी परिचर्चा गुरु की आलोचना तथा साधना में शिथिलता की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाती है। गुरु के उपदेश का अक्षरशः पालन कीजिए। स्मरण रखिए कि वह केवल आपके लिए है। अन्य शिष्यों ने भी गुरूपदेश ग्रहण किया हुआ है। उन्हें उसका पालन करने दीजिए। आपने जो उपदेश प्राप्त किया है, उसे दूसरों पर न थोपिए ।
शिष्य अपनी निष्ठा की मात्रा के अनुपात में ही अपने गुरु से आत्मसात् अथवा प्राप्त करता है। जब गुरु आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए शिष्य के पास आता है, उस समय शिष्य यदि ध्यान नहीं देता, वह यदि अभिमानी और लापरवाह है, यदि वह अपने हृदय-द्वार में अर्गला लगा देता है, तो वह लाभान्वित नहीं होता।
गुरु द्वारा परीक्षा
सद्गुरु बार-बार अनुनय-विनय करने तथा कठोर परीक्षा लेने के पश्चात् ही अपने विश्वस्त शिष्यों को उपनिषद् के गूढ़ रहस्यों को बतलाता है। गुरु कभी-कभी अपने शिष्य को प्रलोभित कर सकता है; किन्तु शिष्य को चाहिए कि गुरु में दृढ़ निष्ठा के द्वारा इसे पार कर जाये।
प्राचीन काल में बहुत ही कठिन परीक्षाएँ ली जाती थीं। एक बार गोरखनाथ ने अपने कुछ शिष्यों को एक ऊँचे वृक्ष पर चढ़ने तथा उनसे शिर के बल नीचे एक तीक्ष्ण त्रिशूल के ऊपर कूदने के लिए कहा। अनेक अविश्वासी शिष्य निश्चल खड़े रह गये; किन्तु एक निष्ठावान् शिष्य तत्काल विद्युत्-गति से वृक्ष पर चढ़ गया और वहाँ से नीचे त्रिशूल पर कूद गया। गोरखनाथ के अदृश्य हाथों ने उसकी रक्षा की। उसे तत्काल आत्म-साक्षात्कार प्राप्त हुआ ।
एक बार वैशाखी के अवसर पर गुरु गोविन्दसिंह ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने कहा : "मेरे प्रिय शिष्यो ! है कोई ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे सके ?” सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। परन्तु पहले एक शिष्य खड़ा हो गया। उसे गुरु अपने खेमे में ले गये। वहाँ पर एक बकरे की बली दे कर खून से सनी तलवार ले कर बाहर आये और बोले— “और कौन धर्म के लिए शीश देने के लिए तैयार है ?” तत्पश्चात् एक के बाद एक चार शिष्यों ने अपने को प्रस्तुत किया और चारों बार वही हुआ जो पहले शिष्य के साथ हुआ था। तदुपरान्त गुरु पाँचों शिष्यों को खेमे से बाहर ले कर आये और उन्हें 'पंच प्यारे' कह कर सम्मानित किया।
गुरु शिष्यों की विविध प्रकार से परीक्षा लेता है। कुछ शिष्य उन्हें गलत समझते हैं और उनमें अपनी निष्ठा खो बैठते हैं। अतः वे लाभान्वित नहीं होते।
चार प्रकार के शिष्य
सर्वोत्तम शिष्य भूतेल (पेट्रोल) अथवा उड्डयन आसव की भाँति होता है। वह बहुत दूर से गुरु के उपदेश के स्फुलिंग के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करता है।
द्वितीय प्रकार का शिष्य कर्पूर की भाँति होता है। एक स्पर्श उसकी अन्तरात्मा को उदबुद्ध बनाता और उसमें आध्यात्मिकता की अग्नि प्रज्वलित करता है।
तृतीय प्रकार का शिष्य कोयले की भाँति होता है। उसमें भाव उत्पन्न करने के लिए गुरु को कठोर श्रम करना पड़ता है।
चतुर्थ प्रकार का शिष्य कदली-स्तम्भ की भाँति होता है। उस पर किया गया कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। गुरु चाहे कुछ भी करे, वह भावशून्य तथा निष्क्रिय बना रहता है।
सुन्दर ढंग से तैयार की हुई मूर्ति अथवा प्रतिमा के लिए दो वस्तुएँ आवश्यक होती हैं। एक है संगमरमर का पूर्ण अनवद्य सुन्दर प्रस्तर-खण्ड तथा दूसरा है निपुण मूर्तिकार । सुन्दर प्रतिमा के उत्कीर्णन तथा तक्षण के लिए संगमरमर-खण्ड को अप्रतिबन्ध रूप से मूर्तिकार के हाथों में रहना चाहिए। इसी भाँति शिष्य को भी अपने को निर्मल तथा शुद्ध करना और पूर्णतया अनिन्द्य संगमरमर का प्रस्तर-खण्ड बनाना चाहिए तथा अपने गुरु के कुशल मार्ग-निर्देशन में रख कर उसे भगवान् की मूर्ति के रूप में उत्कीर्णन तथा तक्षण के लिए खुला छोड़ देना चाहिए ।
तृतीय अध्याय
पावन गुरुपूर्णिमा-दिवस की अर्थवत्ता
शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणम् ।
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ।।
"श्री शंकराचार्य साक्षात् शंकर हैं और वेदव्यास साक्षात् विष्णु-रूप हैं। में ब्रहासूग तथा उसके भाष्यकर्ता — दोनों भगवत्स्वरूपों की बारम्बार वन्दना करता हूँ ।"
(गुरुवन्दनम् )
आषाढ़ मास की पूर्णमासी गुरुपूर्णिमा का अतीव मांगलिक तथा पवित्र दिवस है। महर्षि श्री व्यास भगवान् अथवा श्रीकृष्ण द्वैपायन के स्मृति दिवस इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन संन्यासी स्वाध्याय, वेदान्त-विचार तथा महर्षि व्यास द्वारा रचित अतीव श्लाघ्य ब्रह्मसूत्रों पर प्रवचन करने के लिए एक स्थान पर टिक कर निवास करते हैं। श्री वेदव्यास ने चारों वेदों का सम्पादन तथा अठारह पुराणों, महाभारत और भागवत की रचना कर मानव-जाति की अविस्मरणीय शाश्वत सेवा की है। हम उनके प्रति गम्भीर कृतज्ञता के ऋण से जो ऋणी हैं, उसके परिशोधन का प्रयास उनकी रचनाओं के निरन्तर स्वाध्याय तथा इस कलियुग में मानवता के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने जो उपदेश दिये हैं, उनके आचरण से कर सकते हैं। सभी साधक तथा भक्त गण इस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष के सम्मान में आज के दिन व्यास-पूजा करते हैं, साधक अपने गुरु की पूजा करते हैं; साधु-महात्माओं का सम्मान तथा आतिथ्य-सत्कार किया जाता है तथा गृहस्थी बड़ी श्रद्धा तथा निष्कपटता से दान-पुण्य करते हैं। संन्यासियों का चातुर्मास आज के दिन से ही आरम्भ होता है। संन्यासी वर्षा ऋतु के चार मासों में एक स्थान पर रह कर ब्रह्मसूत्रों का स्वाध्याय तथा निदिध्यासन करते हैं।
इस महत्त्वपूर्ण दिवस की गम्भीर अर्थवत्ता पर पूर्ण ध्यान दें। आषाढ़ पूर्णिमा चातुर्मास अथवा उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षित वर्षा के प्रारम्भ की घोषणा करती है। उष्ण ग्रीष्म ऋतु में कर्षित तथा मेघ के रूप में संचित जल अब प्रचुर वृष्टि के रूप में प्रकट होता है जो सर्वत्र नव-जीवन के आगमन का प्रारम्भक है। इसी भाँति आप सबने भी अपने अध्यवसायी परिशीलन द्वारा जिन सिद्धान्तों तथा तत्त्वज्ञान को अपने में संचित कर रखा है, गम्भीरतापूर्वक उन सबको वास्तविक कार्य रूप में परिणत करना आरम्भ कर दें। आज के दिन से ही व्यावहारिक आध्यात्मिक साधना प्रारम्भ करें। आध्यात्मिकता की नवीन लहरें उत्पन्न करें। जो कुछ आपने पढ़ा, सुना, देखा तथा सीखा है, उस सबको साधना द्वारा विश्व-प्रेम के अविरत भावोद्गार, अविराम प्रेममयी सेवा तथा प्राणियों में विराजमान प्रभु की सतत पूजा तथा प्रार्थना में परिणत होने दें।
आज के दिन दूध तथा फल पर निर्वाह करें और उग्र जप तथा ध्यान का अभ्यास करें। चातुर्मास काल में ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय तथा अपने गुरु-मन्त्र अथवा इष्ट-मन्त्र का कुछ लाख जप का अनुष्ठान अथवा पुरश्चरण करें। इससे आप अत्यधिक लाभान्वित होंगे।
यह दिव्य गुरु-पूजा-दिवस के रूप में सच्चे शिष्य के लिए विशुद्ध आनन्द का दिन है। अपने परम प्रिय गुरु को अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की प्रत्याशा से पुलकित साधक इस अवसर की उत्सुकता तथा श्रद्धा के साथ प्रतीक्षा करते हैं। एकमात्र गुरु ही मोह-पाश को भंग करता तथा साधक को सांसारिक जीवन के बन्धन से मुक्त करता है। श्रुति कहती है
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।।
"जिसकी परमेश्वर में परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में होती है उसी प्रकार अपने गुरु में होती है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं" (श्वेताश्वतर उपनिषद् : ६-२३) । गुरु साक्षात् ब्रह्म है। वह आपकी अन्तरतम सत्ता से आपका पथ-प्रदर्शन करते तथा आपको प्रेरणा देते हैं।
समस्त जगत् को गुरु-स्वरूप देखें
नवीन दृष्टिकोण अपनायें। समस्त जगत् को गुरु-स्वरूप देखें। इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में गुरु के मार्ग-दर्शक कर, उद्बोधक वाणी तथा प्रबोधक संस्पर्श के दर्शन करें। अब समग्र जगत् आपकी परिवर्तित दृष्टि के समक्ष रूपान्तरित रूप में स्थित होगा । विराट् गुरु जीवन के सभी मूल्यवान् रहस्यों का उद्घाटन कर ज्ञान प्रदान करेंगे। दृश्य प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त परम गुरु आपको जीवन की सर्वाधिक उपयोगी शिक्षाएँ प्रदान करेंगे। इन गुरुओं के गुरु की, उस गुरु की जिसने अवधूत दत्तात्रेय को भी उपदेश दिया, नित्य पूजा कीजिए। अपनी उदात्त सहिष्णुता वाली मौन परम सहनशीला पृथ्वी, स्वैच्छिक आत्म-बलिदान करने वाला छायादार फलदायक वृक्ष, नन्हें बीज में धैर्यपूर्वक शान्त पड़ा रहने वाला महान् पीपल, अपने अध्यवसाय से शिलाओं को घिस डालने वाली टपकने वाली बूँदें, सुव्यवस्थित समयनिष्ठ तथा नियमनिष्ठ ग्रह तथा ऋतुएँ — ये सब उनके लिए दिव्य गुरु हैं जो देखता, सुनता तथा ग्रहण करता है।
शुद्धता एवं उन्नति
ग्रहणशीलता के मूर्त रूप बनें। अपनी क्षुद्र अहं भावना से अपने को रिक्त बनायें । प्रकृति के वक्षस्थल में बन्द समस्त निधि आपकी हो जायेगी। आप अल्प काल में ही आश्चर्यजनक उन्नति तथा पूर्णता प्राप्त करेंगे। पर्वतीय समीर की भाँति शुद्ध तथा अनासक्त बनें। जैसे सरिता अपने लक्ष्य सागर की ओर अनवच्छिन्न, अनवरत तथा निरन्तर प्रवाहित होती है, वैसे ही आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सच्चिदानन्द की परमावस्था की ओर गति करके अपने सभी विचार, वाणी और कर्म को केवल चरम लक्ष्य की ओर निर्देशित करें।
चन्द्रमा सूर्य के चकाचौंध करने वाले प्रकाश को प्रतिबिम्बित कर चमकाता है। पूर्णिमा का राकेन्दु ही सूर्य के तेजस्वी प्रकाश को उसके पूर्ण वैभव में प्रतिबिम्बित करता है। वह सूर्य को महिमान्वित करता है। सेवा तथा साधना की अग्नि द्वारा अपने को शुद्ध बनायें तथा राकेश की भाँति आत्मा के तेजस्वी प्रकाश को प्रतिबिम्बित करें। प्रकाशों के प्रकाश ब्रह्म-वैभव के पूर्ण परावर्तक बनिए। देदीप्यमान सूर्यों के सूर्य, दिव्यता के जीवन-साथी बनने को अपना लक्ष्य बनाइए ।
तत्त्वमसि
एकमात्र ब्रह्म अथवा परमात्मा ही सत् है। वह सबका आत्मा है। वह सर्वस्व है। वह इस ब्रह्माण्ड का सारतत्त्व है। वह ऐसा अद्वैत तत्त्व है जो प्रकृति की सभी विविधताओं तथा भिन्नताओं में कभी भी द्वैत स्वीकार नहीं करता। आप वही अमर, सर्वव्यापक, सर्वानन्दमय ब्रह्म हैं। तत्त्वमसि —तुम वही (ब्रह्म) हो। इसका साक्षात्कार करें तथा मुक्त बनें।
ब्रह्मसूत्र के ये चार महत्त्वपूर्ण सूत्र स्मरण रखें :
(१) अथातो ब्रह्मजिज्ञासा- अब यहाँ से ब्रह्म-विषयक विचार आरम्भ किया जाता है (१-१-१);
(२) जन्माद्यस्य यतः इस जगत् के जन्मादि जिससे होते हैं (१-१-२);
(३) शास्त्र योनित्वात् — शास्त्र में ब्रह्म को जगत् का कारण बताया गया है (१-१-३); तथा
(४) तत्तु समन्वयात्—वह ब्रह्म समस्त जगत् में अनुगत होने से (उपादान भी है) (१-१-४)।
अब गायें :
जय परम गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम ।
जगद्गुरु गुरु सद्गुरु श्याम ।।
श्री व्यास तथा ब्रह्मविद्यागुरुओं को स्मरण करें तथा उनकी पूजा करें। आप सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो! आप सब अविद्या-ग्रन्थि का उच्छेदन कर भाग्यशाली जीवन्मुक्तों की भाँति सर्वत्र शान्ति, आनन्द तथा प्रकाश विकीर्ण करते हुए देदीप्यमान हों!
चतुर्थ अध्याय
महर्षि व्यास तथा हिन्दू-शास्त्रों को उनका योगदान
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र ।
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ।।
"हे प्रस्फुटित पद्म-पत्र सदृश नेत्र विशिष्ट महामति व्यास आपको नमस्कार; जिसने महाभारत सदृश तैल द्वारा परिपूर्ण ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वलित किया है।"
(गीताध्यानम् )
प्राचीन काल में हमारे पूर्वज, आर्यावर्त के ऋषिजन व्यासपूर्णिमा- जो कि हिन्दू-पंचांग में एक विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण दिवस है—के उत्तरवर्ती चार महीनों में तपस्या करने के लिए वन में चले जाया करते थे। इस स्मरणीय दिवस को ही भगवान् के अवतार व्यास जी ने अपने ब्रह्मसूत्रों की रचना आरम्भ की थी। हमारे प्राचीन ऋषि यह तपस्या गुहाओं तथा वनों में करते थे; किन्तु अब समय परिवर्तित हो चला है और यद्यपि ऐसे गृहस्थ तथा राजा अविद्यमान नहीं हैं जो ऐसी सहायता तथा सुविधाएँ जो वे प्रदान कर सकते हैं, चतुर्थ आश्रमियों के अधिकार में देने को समर्थ तथा उत्सुक हैं, पर ऐसी सुविधाएँ अब सर्वसुलभ नहीं रही हैं। वनों एवं गुहाओं का स्थान उनके गुरुद्वारों और मठों के कुटीरों ने ले लिया है। व्यक्ति को अब आवश्यकतावश अपने को स्थानों तथा समयों के उपयुक्त बनाना होगा। स्थान तथा परिस्थिति के परिवर्तन से हमारी मानसिक अभिवृत्ति में इतना अधिक अन्तर नहीं आने देना चाहिए। चातुर्मास व्यासपूर्णिमा-दिवस से आरम्भ होता है। शास्त्र के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम इस दिन व्यास तथा ब्रह्मविद्या-गुरुओं की पूजा करें तथा ब्रह्मसूत्रों और अन्य आर्ष ग्रन्थों का स्वाध्याय आरम्भ कर दें।
कृष्णद्वैपायन का जन्म
हमारे पुराण अनेक व्यासों का उल्लेख करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग के अन्त में प्रस्तुत व्यास–कृष्णद्वैपायन—के जन्म लेने से पूर्व अट्ठाईस व्यास हो चुके थे। उनका जन्म कुछ विलक्षण तथा असाधारण परिस्थितियों में पराशर ऋषि के द्वारा मत्स्य-कन्या सत्यवती से हुआ। पराशर परम ज्ञानी तथा फलित ज्योतिष के सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक थे। उन द्वारा रचित 'पाराशर होरा' आज भी फलित ज्योतिष का पाठ्य-ग्रन्थ है। उन्होंने 'पाराशर स्मृति' के नाम से एक स्मृति ग्रन्थ की भी रचना की। इसे इतना अधिक सम्मान प्राप्त है कि मानव-विज्ञान तथा नीति-शास्त्र के वर्तमान कालिक लेखक इसका उद्धरण देते हैं। पराशर को पता चला कि अमुक घटिका में गर्भधारण करने वाला बालक महत्तम युगपुरुष के रूप में जन्म लेगा। इतना ही नहीं, वह साक्षात् भगवान् विष्णु का अंश होगा। उस दिन पराशर ऋषि नौका द्वारा यात्रा कर रहे थे। उन्होंने नाविक को इस आसन्न शुभ घड़ी के सम्बन्ध में बतलाया। नाविक के एक विवाहोपयुक्त वयस्क पुत्री थी। वह ऋषि की सन्तता तथा महत्ता से प्रभावित हो गया। उसने पराशर को विवाह में अपनी पुत्री भेंट कर दी। इस युग्मन से हमारे व्यास का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनका जन्म स्वयं भगवान् शिव के आशीर्वाद से हुआ जिन्होंने एक उच्च कोटि के ज्ञानी ऋषि का एक निम्न कुलोत्पन्न कन्या से संयोग को आशीर्वाद दिया था।
हिन्दू-शास्त्रों को उनका महान् योगदान
अत्यल्पवयस्कावस्था में ही व्यास ने अपने माता-पिता को अपने जीवन के रहस्य से अवगत करा दिया था कि वे वन में जा कर अखण्ड तप करेंगे। उनकी माता प्रथम तो सहमत नहीं हुई; किन्तु बाद में उन्होंने इस आवश्यक प्रतिबन्ध पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी कि जब कभी उनको उनकी उपस्थिति की इच्छा हो, वे उनके सम्मुख प्रकट हो जायें। यह स्वयं इस बात को व्यक्त करता है कि माता-पिता तथा पुत्र कितने दूरदर्शी थे। पुराणों का कथन है कि व्यास ने अपने इक्कीसवें गुरु वसुदेव ऋषि से दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने सनक तथा सनन्दन ऋषियों तथा अन्य लोगों से शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने मानव हितार्थ वेदों का वर्गीकरण किया तथा श्रुतियों के आशु तथा सहज बोध के लिए ब्रह्मसूत्रों की रचना की। उन्होंने महाभारत का भी प्रणयन किया जिससे कि स्त्रियाँ, शूद्र तथा अन्य अल्पतर बुद्धि वाले लोग परमोत्कृष्ट ज्ञान को सरलतम विधि से हृदयंगम कर सकें। उन्होंने अठारह पुराणों की रचना की तथा उपाख्यानों द्वारा उनको समझाने की शैली संस्थापित की। इस भाँति उन्होंने तीन मार्गों अर्थात् कर्म, उपासना तथा ज्ञान की स्थापना की। उन्हें यह भी श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने अपनी माँ की वंश-परम्परा बनाये रखी तथा धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुर उनकी सन्तान हैं। व्यास की अन्तिम कृति भागवत है जिसकी रचना उन्होंने देवर्षि नारद की प्रेरणा से की। देवर्षि नारद एक बार उनके यहाँ आये और उन्हें इसको लिखने के लिए परामर्श दिया; क्योंकि इसके बिना वे अपने जीवन-लक्ष्य को न पहुँच पाते।
सभी हिन्दू व्यास को चिरंजीवि मानते हैं। वे अब भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए संसार भर में विचरण करते रहते हैं और सच्चे तथा निष्ठावान् भक्तों के सम्मुख प्रकट भी होते हैं। कहा जाता है कि जगद्गुरु शंकराचार्य ने मण्डन मिश्र के घर में उनके दर्शन किये तथा वे अन्य अनेक लोगों के सम्मुख भी प्रकट हुए। इस भाँति संक्षेप में कहें तो वे संसार के कल्याण के लिए रहते हैं। आइए, हम सब प्रार्थना करें कि हम सब पर तथा समग्र विश्व पर उनका आशीर्वाद रहे !
ब्रह्मसूत्र तथा उन पर विविध भाष्य
प्रत्येक व्यक्ति को यह सुविदित है कि हमारे पूर्वजों ने छह महत्त्वपूर्ण शास्त्रों का विकास किया, जिन्हें षड्दर्शन अर्थात् सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा अर्थात् वेदान्त कहते हैं। प्रत्येक दर्शन के विचारों में सूक्ष्म भेद है। कालान्तर में ये विचार अपरिचालनीय हो चले, जिससे उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए सूत्रों का आविर्भाव हुआ । लघु सूक्तियों में, जिन्हें संस्कृत में सूत्र कहते हैं, निबन्ध लिखे गये। सूत्र का अर्थ है स्मृति-संकेत अथवा प्रत्येक विषय पर लम्बी परिचर्चाओं के सहायक। पद्मपुराण में सूत्र शब्द की परिभाषा दी गयी है कि सूत्र संक्षिप्त तथा असन्दिग्ध होना चाहिए; किन्तु संक्षिप्तता इस सीमा तक लायी गयी कि सूत्र अबोधगम्य हो गया। यह बात ब्रह्मसूत्रों के विषय में विशेष सत्य है। आज हम एक ही सूत्र के दर्जनों प्रकार से भाष्य करते हुए पाते हैं। व्यास अथवा बादरायण (यह व्यास का एक अतिरिक्त नाम था) कृत ब्रह्मसूत्र 'वेदान्तसूत्र' के नाम से भी प्रसिद्ध है; क्योंकि उनमें केवल वेदान्त पर ही विचार किया गया है। वे चार अध्यायों में विभाजित हैं जिनमें से प्रत्येक को पुनः चार पादों में उपविभाजित किया गया है। यह ध्यान देने योग्य रोचक बात है कि उनका आरम्भ 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' सूत्र से और अन्त 'अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्' सूत्र से होता है, जिन्हें एक-साथ मिला कर पढ़ने पर अर्थ होता है : "ब्रह्म के स्वरूप की जिज्ञासा", "वापस नहीं आता है।" अर्थात् "उस मार्ग से चल कर व्यक्ति अमरत्व प्राप्त करता है" और "वह फिर संसार में वापस नहीं आता।" इन सूत्रों के कृतित्व के सम्बन्ध में, परम्परागत विश्वास इसे व्यास का ही मानता है। शंकराचार्य अपने भाष्य में व्यास का उल्लेख गीता तथा महाभारत के रचयिता के रूप में तथा बादरायण का ब्रह्मसूत्रों के रचयिता के रूप में करते हैं। वाचस्पति, आनन्दगिरि तथा उनके अन्य अनुयायी दोनों को एक ही व्यक्ति मानते हैं, जब कि रामानुज तथा अन्य इसके कृतित्व को व्यास का ही मानते हैं। ब्रह्मसूत्रों पर प्राचीनतम भाष्य शंकराचार्य का है। बाद में वल्लभ, रामानुज, निम्बार्क, मध्व तथा अन्य लोगों ने उनका अनुसरण किया और अपने-अपने वाद स्थापित किये। उनमें से मुख्य, जिनकी संख्या, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, पाँच है, इन दो विषयों में प्रायः सहमत हैं। अर्थात् (१) ब्रह्म इस जगत् का कारण है, और (२) ब्रह्मज्ञान मोक्ष प्राप्त कराता है। किन्तु ब्रह्म के स्वरूप, जीवात्मा के तथा परमात्मा के सम्बन्ध तथा मुक्तात्मा की दशा के विषय में उनमें परस्पर मतभेद हैं। उनमें से कुछ लोगों के अनुसार मोक्ष-प्राप्ति का मुख्य साधन भक्ति है, ज्ञान नहीं जैसा कि शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया है।
व्यास का जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति का अनुपम उदाहरण है। उनकी कृतियाँ आज भी हमें तथा समग्र विश्व को प्रेरणा प्रदान करती हैं। अच्छा हो कि हम उनकी कृतियों की भावनाओं के अनुरूप जीवन-यापन करें।
पंचम अध्याय
श्री दक्षिणामूर्ति
निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिनाम् ।
गुरवे सर्वलोकानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः ।।
" श्री दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है जो सब विद्याओं के आगार है, भवरोग से पीड़ित सभी लोगों के लिए वैद्य तथा सभी के गुरु हैं।"
(गुरुगीता)
भगवान् शिव पार्श्व में पार्वती देवी के साथ कैलास पर्वत पर मणियों से रमणीय ढंग से सुसज्जित मण्डप में आसीन थे। इस समय देवी ने भगवान् की पूजा की तथा दक्ष-पुत्री होने के कारण उनका पहले जो दाक्षायणी नाम पड़ा था, उसे परिवर्तित करने की उनसे प्रार्थना की। दक्ष को भगवान् शिव ने उनके अनादर तथा दर्प के कारण मार डाला था। भगवान् शिव ने देवी की यह प्रार्थना सुन कर उन्हें आदेश दिया कि वह सन्तान प्राप्त्यर्थ उग्र तप कर रहे पर्वतराज की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण करें। उन्होंने पार्वती से यह भी कहा कि वे उनके साथ विवाह करने उनके पास पधारेंगे। इस प्रकार आज्ञा पा कर पार्वती देवी ने पर्वतराज की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया और भगवान् शिव की वधू बनने के लिए अपने पाँचवें वर्ष की वय में कठोर तप करना आरम्भ कर दिया।
देवी की अनुपस्थिति से जब भगवान् शिवजी अकेले थे, तब ब्रह्मा के पुत्र—सनक, सनन्दन, सनानत और सनत्कुमार भगवान् शिवजी के दर्शनार्थ पधारे और उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया। उन्होंने भगवान् से उन्हें अविद्या को विदूरित करने तथा मोक्ष-प्राप्ति की विधि की शिक्षा देने की प्रार्थना की। उन्होंने बतलाया कि शास्त्र-ग्रन्थों के विशद परिशीलन के बावजूद भी उन्हें मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं हुई तथा उन्हें अन्तरस्थ रहस्य को जानने की आवश्यकता है जिसको जान लेने पर वे मोक्ष प्राप्त कर सकें।
भगवान् शिव ने ऋषियों की प्रार्थना सुन कर दक्षिणामूर्ति का रूप धारण कर लिया और परम गुरु के रूप में रह कर मौन धारण तथा अपने हाथ से चिन्मुद्रा-प्रदर्शन द्वारा उन्हें अन्तरस्थ रहस्य का ज्ञान देना प्रारम्भ कर दिया। भगवान् द्वारा प्रदर्शित विधि से ऋषियों ने ध्यान करना आरम्भ कर दिया तथा अवर्णनीय और असीम आनन्द की अवस्था प्राप्त की।
इस भाँति भगवान् शिव दक्षिणामूर्ति-नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान् दक्षिणामूर्ति का आशीर्वाद हम सब पर हो ! आप सब उनकी कृपा से गहरा अवगाहन करें तथा शाश्वत शान्ति और आनन्द का उपभोग करें!
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!
षष्ठ अध्याय
भगवान् दत्तात्रेय तथा उनके चौबीस गुरु
आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः
मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोऽस्तु ते ।
ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले
प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेयाय नमोऽस्तु ते ॥
"भगवान् दत्तात्रेय को नमस्कार है जो त्रिमूर्तिस्वरूप हैं, जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अन्त में सदाशिव हैं । भगवान् दत्तात्रेय को बारम्बार नमस्कार है जिनकी मुद्रा ब्रह्मज्ञान है, जिनके वस्त्र आकाश तथा भूतल हैं तथा जो साकार प्रज्ञानघन हैं।'
(श्री शंकराचार्य)
अनसूया को प्रायः सतीत्व के प्रतिमान के रूप में उद्धृत किया जाता है। वे महर्षि अत्रि की पत्नी थीं, जो एक महान् ऋषि तथा सप्तर्षियों में से एक थे। वे पातिव्रत-धर्म में सुस्थित थीं तथा अपने पति की भाव-प्रवण सेवा करती थीं। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव-तुल्य पुत्र प्राप्त करने के लिए सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या की।
एक बार नारद जी चने के दाने के बराबर लोहे की एक छोटी गोली ले कर सरस्वती देवी के पास गये और उनसे कहा: "हे सरस्वती देवी! कृपया इस लोहे की गोली को भून दीजिए। मैं यात्रा-काल में इस लोहे के चने को खाऊँगा।” सरस्वती देवी हँस पड़ी और कहा: "हे नारद ऋषि! यह लोहे की गोली क्योंकर भूनी जा सकती है? यह कैसे खायी जा सकती है?" तत्पश्चात् नारद जी महालक्ष्मी तथा पार्वती देवी के पास गये और उनसे लोहे की गोली को भूनने की प्रार्थना की। वे भी नारद ऋषि पर हँस पड़ी। तब नारद जी ने कहा "हे देवियो देखें, मैं इसे अत्रि महर्षि की पत्नी अनसूया से भुनवाऊँगा। वे परम पतिव्रता हैं तथा भूलोक में रहती हैं।"
तब नारद जी अनसूया के पास आये और उनसे लोहे के बने को भूनने की प्रार्थना की। अनसूया से लोहे की गोली को एक कड़ाही में डाल दिया, अपने पतिदेव के रूप का ध्यान किया तथा उनके चरणोदक की कुछ बूँदें लोहे की गोली के ऊपर छिड़क दीं। वह तुरन्त भुन गयी। नारद सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती के पास गये, उनके सम्मुख भुने हुए लोहे के चने खाये तथा उसमें से थोड़ा-सा उन्हें भी दिया। उन्होंने अनसूया के तेज तथा सतीत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की। तब नारद ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव-तुल्य पुत्रों को जन्म देने की अनसूया की इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया।
उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती से कहा: “यदि आप सबने श्रद्धा, शुद्ध हृदय तथा भक्तिपूर्वक अपने-अपने पतियों की सेवा की होती, तो आप भी लोहे की गोली को भून सकती थीं। अपने पतियों से अनसूया के पातिव्रत की परीक्षा लेने की प्रार्थना कीजिए।"
तब सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने अपने-अपने पतियों से अत्रि महर्षि की पत्नी अनसूया के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेने तथा उनसे निर्वाण भिक्षा-नग्नावस्था में दान लेने के लिए प्रार्थना की।
त्रिमूर्तियों को ज्ञान दृष्टि से नारद की करतूत तथा अनसूया के तप और मनोकामना का पता चल गया। वे सहमत हो गये। त्रिमूर्तियों ने संन्यासी का वेश धारण किया, अनसूया के सम्मुख प्रकट हुए तथा उनसे उन्हें निर्वाण भिक्षा देने की याचना की। अनसूया बड़े धर्मसंकट में पड़ 'गयीं। वे भिक्षुओं को 'न' नहीं कह सकती थीं। उन्हें अपने पातिव्रत धर्म का पालन भी करना था। उन्होंने अपने पति के रूप का ध्यान किया, उनके चरणों की शरण ली और अपने पति के चरणोदक को तीनों संन्यासियों के ऊपर छिड़क दिया। उस चरणामृत के प्रताप के कारण त्रिमूर्ति तीन शिशुओं में रूपान्तरित हो गये। उसी समय अनसूया के स्तनों में दुग्ध भर आया। उन्होंने इन शिशुओं को अपना ही शिशु समझा और नग्नावस्था में उन्हें दुग्ध-पान कराया और उन्हें पालने में सुला दिया। वे अपने पति, जो स्नानार्थ बाहर गये थे, के आगमन की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगीं।
अत्रि ऋषि ज्यों ही घर वापस आये, अनसूया ने उनकी अनुपस्थिति में जो-कुछ घटित हुआ था, सब अपने पति से कह सुनाया, उनके चरणों में तीनों शिशुओं को रख दिया तथा उनकी (ऋषि की) पूजा की। किन्तु अत्रि को अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब बातें पहले ही ज्ञात हो चुकी थीं। उन्होंने तीनों शिशुओं का आलिंगन किया। वे तीनों शिशु दो पैर, एक धड़, तीन शिर तथा छह हाथों से युक्त एक शिशु बन गया। अत्रि ऋषि ने अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया और उसे अवगत किया कि उनकी कामना की तुष्टि के लिए त्रिमूर्तियों ने ही तीन शिशुओं का रूप धारण कर रखा है।
नारद ब्रह्मलोक, वैकुण्ठ और कैलास गये तथा सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को सूचित किया कि उनके पतियों ने जब अनसूया से निर्वाण-भिक्षा माँगी, तो वे उनके पातिव्रत-धर्म की शक्ति से शिशुओं के रूप में परिवर्तित हो गये हैं और यदि वे अत्रि से भर्तृ-भिक्षा नहीं माँगेंगीं, तो वे वापस नहीं आयेंगे। सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती ने सामान्य स्त्रियों का रूप धारण किया, अत्रि के सम्मुख प्रकट हुईं और भर्तृ-भिक्षा की याचना की : “हे ऋषि! कृपया हमारे पतियों को हमें वापस दें।” अत्रि ने तीनों देवियों का यथोचित सम्मान किया तथा करबद्ध हो कर उनसे प्रार्थना की कि उनकी तथा अनसूया की इच्छा पूर्ण हो! अब त्रिमूर्ति अत्रि के समक्ष अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहा: “आपके कथनानुसार यह बालक एक महान् ऋषि और अनसूया के इच्छानुसार हमारे समान होगा। इस बालक का नाम दत्तात्रेय होगा।" तत्पश्चात् वे अन्तर्धान हो गये।
दत्तात्रेय प्रौढ़ हुए। क्योंकि उनमें त्रिमूर्तियों के अंश थे और वे एक महान् ज्ञानी थे, इसलिए सभी ऋषि तथा तपस्वी उनकी पूजा करते थे। वे सौम्य, शान्त तथा स्नेही थे। उनके पीछे लोगों की बहुत बड़ी भीड़ सदा लगी रहती थी। दत्तात्रेय उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे; किन्तु उनके सभी प्रयास विफल रहे। एक बार जब वे अनेक लोगों से घिरे थे, वे स्नानार्थ एक नदी में प्रवेश कर गये और उसमें से तीन दिन तक बाहर नहीं निकले। वे जल के अन्दर समाधिस्थ हो गये। तीसरे दिन जब वे बाहर आये, तो उन्होंने देखा कि लोग उनके वापस आने की प्रतीक्षा में तब भी सरिता-तट पर बैठे हुए थे।
वे इस उपाय से लोगों से अपना पिण्ड छुड़ाने में सफल न हुए। उन्होंने अन्य विधि अपनायी। उन्होंने अपनी योग-शक्ति से एक सौन्दर्यवती किशोरी तथा एक बोतल सुरा उत्पन्न की। वे एक हाथ से उस किशोरी को तथा दूसरे हाथ में सुरा की बोतल पकड़े हुए जल से बाहर निकले। लोगों ने समझा कि दत्तात्रेय योग-भ्रष्ट हो गये हैं; अतः वे उन्हें छोड़ कर चले गये ।
दत्तात्रेय ने अपनी सभी वैयक्तिक सम्पत्ति को, यहाँ तक कि उनके पास जो नाम मात्र का वस्त्र था, उसे भी त्याग दिया और अन्त में अवधूत बन गये। वे वेदान्त के सत्यों की शिक्षा तथा उपदेश देने बाहर निकल पड़े। दत्तात्रेय ने 'अवधूत-गीता' नामक अपनी गीता की शिक्षा भगवान् सुब्रह्मण्यम् या कार्तिकेय को दी। यह बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है। इसमें वेदान्त के सत्य तथा रहस्य और आत्मा की अपरोक्षानुभूति अन्तर्विष्ट है।
एक बार जब दत्तात्रेय वन में आनन्दपूर्वक विचरण कर रहे थे, उनकी भेंट राजा यदु से हुई। यदु ने उन्हें अत्यन्त आनन्दित देख कर उनसे उनके आनन्द का रहस्य तथा उनके गुरु का नाम जानना चाहा। दत्तात्रेय ने कहा : "आत्मा ही मेरा गुरु है, तथापि मैंने चौबीस व्यक्तियों से शिक्षा ग्रहण की अतः से मेरे गुरु हैं।"
तब दत्तात्रेय जी ने अपने चौबीस गुरुओं के नाम तथा उनमें से प्रत्येक से ग्रहण की हुई शिक्षाओं का उल्लेख किया।
मेरे चौबीस गुरुओं के नाम हैं:
(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) वायु, (४) अप्रि, (५) आकाश, (६) चन्द्रमा, (७) सूर्य, (८) कपोत, (९) अजगर, (१०) समुद्र, (११) पतंग, (१२) मधुमक्खी, (१३) शहद निकालने वाला, (१४) हाथी, (१५) हरिन, (१६) मछली, (१७) पिंगला वेश्या, (१८) कुरर पक्षी, (१९) चालक, (२०) कुमारी कन्या, (२१) सर्प, (२२) बाण बनाने वाला, (२३) मकड़ी तथा (२४) भृंगी कीट।
(१) मैंने पृथ्वी से धैर्य तथा परोपकार की शिक्षा ली है; क्योंकि वह लोगों द्वारा अपने ऊपर किये गये सभी आघातों को सहन करती है और बदले में शस्य, फल आदि उत्पन्न कर उनका हित करती है।
(२) जल से मैंने पवित्रता की शिक्षा ली है। जैसे शुद्ध जल दूसरों को स्वच्छ बनाता है वैसे ही निष्कल्मष तथा स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि से मुक्त सन्त अपने सम्पर्क में आने वाले सभी को पवित्र बनाता है।
(३) वायु सदा अनेक पदार्थों से हो कर प्रवाहित होता रहता है, परन्तु वह उनमें से किसी से भी आसक्त नहीं होता; अतः मैंने वायु से अनासक्त रहने की शिक्षा ग्रहण की है, यद्यपि मैं इस संसार में अनेक लोगों के मध्य में विचरण करता रहता हूँ।
(४) जैसे अभि प्रज्वलित होने पर ज्योतिर्मय होती है, वैसे ही सन्त पुरुष को अपने ज्ञान तथा तपस्या की आभा से देदीप्यमान होना चाहिए।
(५) वायु, तारे, मेघ आदि सभी आकाश में अन्तर्विष्ट हैं; किन्तु आकाश इनमें से किसी के भी सम्पर्क में नहीं आता है। मैंने आकाश से यह शिक्षा ली है कि आत्मा सर्वव्यापक है, तथापि वह किसी पदार्थ के सम्पर्क में नहीं आता है।
(६) यद्यपि चन्द्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी के परिवर्ती प्रतिबिम्ब के कारण वह घटता-बढ़ता-सा प्रतीत होता है; पर वह सदा पूर्ण ही रहता है। मैंने चन्द्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि आत्मा सदा ही पूर्ण तथा निर्विकार है। केवल उपाधियाँ ही उसे आच्छादित करती हैं।
(७) जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य अनेक प्रतिबिम्बों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही ब्रह्म भी मन द्वारा प्रतिबिम्बित उपाधियों (शरीरों) के कारण भिन्न-भिन्न दिखलायी पड़ता है। यह शिक्षा मैंने सूर्य से ग्रहण की।
(८) एक बार मैंने एक कपोत दम्पति को अपने बच्चों के साथ देखा । व्याध ने जाल फैलाया और बच्चों को पकड़ लिया। कपोती को अपने बच्चों में बहुत राग था। वह अब जीना नहीं चाहती थी, अतः वह जाल में जा गिरी और पकड़ी गयी। कपोत कपोती पर अनुरक्त था, अतः वह भी जाल में जा गिरा और पकड़ा गया। इन सबसे मैंने यह शिक्षा ली कि राग ही बन्धन का कारण है।
(९) अजगर भोजन के लिए कोई चेष्टा नहीं करता है। जो कुछ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है, उससे सन्तुष्ट रह कर वह एक स्थान पर पड़ा रहता है। इससे मैंने शिक्षा ली कि भोजन के विषय में उदासीन रहे और • प्रारब्ध से प्राप्त भोजन से सन्तुष्ट रहे (अजगर-वृत्ति) ।
(१०) जैसे समुद्र में सैकड़ों नदियाँ गिरती हैं, किन्तु वह उनसे अप्रभावित रहता है; वैसे ही सुधी व्यक्ति को सभी प्रकार के प्रलोभनों, कठिनाइयों तथा कष्टों में शान्त रहना चाहिए। यह शिक्षा मैंने समुद्र से ग्रहण की।
(११) जैसे पतंग अभि की चमक पर मोहित हो कर उसमें कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही वासनामय पुरुष जो सुन्दरी किशोरी के प्रेम-पाश में पड़ता है, शोक को प्राप्त होता है। मैंने पतंग से दृगेन्द्रिय को नियन्त्रित करने तथा मन को आत्मा पर केन्द्रित करने की शिक्षा ली है।
(१२) जैसे मधुमक्खी एक ही पुष्प से रस न चूस कर विभिन्न पुष्पों से रस चूसती है, वैसे ही मैं भी थोड़ी भिक्षा एक घर से और थोड़ी भिक्षा दूसरे घर से ले कर अपनी क्षुधा शान्त करता हूँ (मधुकरी-भिक्षा अथवा मधुकरी-वृत्ति)। मैं गृहस्थ के लिए भार नहीं बनता हूँ।
(१३) मधुमक्खियाँ बहुत कष्ट उठा कर मधु-संचय करती हैं, किन्तु शहद निकालने वाला आता है और बड़ी सरलतापूर्वक मधु ले कर चलता बनता है; वैसे ही लोग बड़ी कठिनाई से धनादि का संचय करते हैं, किन्तु जब काल आ कर उन पर अधिकार करता है तो उन्हें उन सबको तत्काल छोड़ कर प्रयाण कर जाना होता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि पदार्थों का संग्रह व्यर्थ ही है।
(१४) हाथी कागज की हथिनी को देख कर कामान्ध हो तिनके से आच्छादित गर्त में जा गिरता है। वह पकड़ा जाता है, बाँधा जाता है तथा अंकुश के द्वारा उत्पीड़ित होता है। वैसे ही कामुक व्यक्ति स्त्रियों के जाल में पड़ कर दुःख भोगते हैं। अतएव काम-वासना को नष्ट करना चाहिए। यह शिक्षा मैंने हाथी से ग्रहण की।
(१५) संगीत से राग होने के कारण हरिन व्याध के प्रलोभन में आ कर जाल में बँध जाता है। इसी भाँति व्यक्ति दुश्चरित्र स्त्रियों के गीत से आकर्षित हो कर विनाश को प्राप्त होता है। व्यक्ति को कामुक गीत कभी भी नहीं सुनना चाहिए। यह शिक्षा मैंने हरिन से ली है।
(१६) जैसे भोजन की लोभी मछली सरलता से चारे का शिकार बनती है वैसे ही जो मनुष्य स्वादलोलुप और अपनी रसनेन्द्रिय के वशीभूत होता है, वह अपनी स्वतन्त्रता खो बैठता है और अनायास ही विनाश को प्राप्त होता है। अतएव भोजन की लोलुपता को नष्ट करना चाहिए। यह शिक्षा मैंने मछली से ग्रहण की है।
(१७) विदेह नगरी में पिंगला नाम की एक वैश्या रहती थी। एक रात्रि वह ग्राहकों की प्रतीक्षा करते-करते ऊब गयी। वह निराश हो गयी। तब उसके पास जो कुछ था, उसने उसी से सन्तोष कर लिया और गम्भीर निद्रा में सो गयी। मैंने उस पतिता स्त्री से यह शिक्षा ली कि आशा का त्याग सन्तोषप्रदायक होता है।
(१८) एक कुरर पक्षी अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लिये दूसरे पक्षियों ने उसका पीछा किया और उसे चोंच से मारने लगे। उस कुरर हुए था। पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे शान्ति तथा विश्रान्ति मिली। मैंने इससे यह शिक्षा ली कि सांसारिक मनुष्य जब ऐन्द्रिक सुखों के पीछे दौड़ता है, तो उसे सभी प्रकार के कष्ट तथा दुःख झेलने पड़ते हैं; परन्तु जब वह ऐन्द्रिक सुखों को त्याग देता है, तो वह उस कुरर पक्षी की तरह सुखी हो जाता है।
(११) स्तन-पान करने वाला शिशु सभी चिन्ताओं, चित्तोद्वेगों तथा आकुलताओं से मुक्त तथा सदा आनन्द-मग्न रहता है। मैंने शिशु से आनन्दमनता के गुण की शिक्षा ग्रहण की।
(२०) एक किशोरी कन्या के माता-पिता उसके लिए उपयुक्त वर खोजने के लिए बाहर गये हुए थे। वह किशोरी घर में अकेली थी। उसी उद्देश्य से माता-पिता की अनुपस्थिति में, उसके विवाह के प्रस्ताव के सन्दर्भ में उसे वरण करने के लिए कई लोग उसके घर आये। उसने स्वयं उनका आतिथ्य सत्कार किया। वह धान कूटने के लिए घर के अन्दर गयी। धान कूटते समय उसकी दोनों कलाइयों में पड़ी शीशे की चूड़ियाँ जोर-जोर से बज रही थीं। बुद्धिमती कुमारी ने सोचा : "चूड़ियों के शब्द से लोगों को पता लग जायेगा कि मैं स्वयं धान कूट रही हूँ और यह कि मेरा परिवार इतना निर्धन है कि वह इस कार्य को करने के लिए दूसरे लोगों को नहीं रख सकता। दोनों हाथों में दो-दो चूड़ियों को छोड़ कर मुझे अपनी शेष चूड़ियाँ तोड़ डालनी चाहिए।" तदनुसार उसने प्रत्येक हाथ में दो-दो चूड़ियाँ छोड़ कर सभी चूड़ियाँ तोड़ डालीं। वे दो-दो चूड़ियाँ भी बहुत बजती थीं। तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी। यद्यपि वह धान कूटती रही, पर तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। मैंने उस कुमारी के अनुभव से निम्न शिक्षा ग्रहण की : जब बहुत लोग एक-साथ रहते हैं तब मतभेद, विक्षोभ, विवाद तथा कलह होता है और दो व्यक्ति भी साथ रहते हैं तब भी अनावश्यक बातचीत तथा अनबन तो होती ही है। तपस्वी अथवा संन्यासी को निर्जन स्थान में अकेले रहना चाहिए।
(२१) साँप अपना बिल नहीं बनाता। वह दूसरों के बनाये हुए बिल में रहता है। उसी भाँति तपस्वी अथवा संन्यासी को अपने लिए घर नहीं बनाना चाहिए। उसे दूसरों की बनायी हुई गुहाओं अथवा मठों में रहना चाहिए। मैंने सर्प से यही शिक्षा ली है।
(२२) एक बार एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण को तीक्ष्ण तथा सीधा करने में जब तन्मय था, तब उसकी दुकान के सामने से ही दल-बल के साथ राजा की सवारी निकल गयी। कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति ने कारीगर के पास आ कर पूछा कि क्या राजा उसकी दुकान के पास से गये हैं? कारीगर ने उत्तर दिया कि उसने कुछ नहीं देखा। वस्तुतः कारीगर का मन अपने काम में पूर्णतः तल्लीन था। इससे उसे यह पता नहीं चला कि.. उसकी दुकान के सामने से कौन जा रहा है। मैंने कारीगर से मन की गहन एकाग्रता के गुण की शिक्षा ग्रहण की है।
(२३) मकड़ी अपने मुख से लम्बा सूत्र निकालती है और उससे जाला बनाती है। वह अपने ही बनाये हुए जाल में फँस जाती है। इसी प्रकार मनुष्य अपने ही विचारों का जाल बुनता है और उसमें उलझ जाता है। मकड़ी से मैंने यह शिक्षा ली कि ज्ञानी पुरुष को सांसारिक विचारों को त्याग कर केवल ब्रह्म-चिन्तन करना चाहिए।
(२४) भृंगी एक कीड़े को पकड़ कर अपने घर में बन्द कर देता है और उसको डंक मारता है। बेचारा कीड़ा भृंगी के लौटने और उसके दंश की आशंका से सदैव उस भृंगी का चिन्तन करता रहता है और स्वयं भृंगी बन जाता है। मनुष्य जिस रूप का बारम्बार चिन्तन करता है, वह काल-क्रम से उसी वस्तु के स्वरूप को प्राप्त होता है। मैंने भृंगी तथा कीट से निरन्तर आत्म-चिन्तन द्वारा स्वयं को आत्मा में रूपान्तरित करने और इस भाँति शरीर से सब प्रकार के मोह त्याग देने तथा मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा ली है।
दत्तात्रेय की शिक्षाओं से राजा बहुत प्रभावित हुए। संसार का त्याग कर आत्मा पर निरन्तर ध्यानाभ्यास करने लगे।
दत्तात्रेय सभी प्रकार की असहिष्णुता तथा पूर्वाग्रह से सर्वथा मुक्त थे। उन्होंने जिस स्रोत से ज्ञान प्राप्त हो सका, उसी से उसे प्राप्त किया। सभी जिज्ञासुओं को दत्तात्रेय का अनुसरण करना चाहिए।
सप्तम अध्याय
गुरुपन — एक महाविनाशकारी रोग
जटिलो मुण्डी लुंचितकेशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः ।
पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो उदरनिमित्तं बहुकृत वेशः ।।
"मनुष्य अपने उदर के लिए क्या ही छद्म वेष धारण करता है। कोई शिर पर जटा बढ़ाता है, तो कोई अपने शिर का मुण्डन करा लेता है और अन्य व्यक्ति काषाय वस्त्र धारण करता है। अज्ञानी व्यक्ति देख कर भी नहीं देखता है।"
(श्री शंकराचार्य)
भारतवर्ष जो अद्वैत-दर्शन की पवित्र भूमि रहा है, जिसने जीवन की अभिन्नता तथा चेतना की एकता का प्रतिपादन करने वाले श्री शंकर, दत्तात्रेय, वामदेव तथा जड़भरत को जन्म दिया, वही आज साम्प्रदायिकों से आकीर्ण है। यह क्या ही महान् खेद का विषय है! आज आप कैसी शोचनीय स्थिति देख रहे हैं! आप सागर-तट की सिकता- कणिकाओं की गणना करने में भले ही सफल हो जायें; किन्तु आज भारत में अभिभावी सम्प्रदायों की संख्या की गणना कर पाना अत्यन्त कठिन है। प्रतिदिन ही एक-न-एक प्रकार का वाद पहले से ही यहाँ वर्तमान फूट को बढ़ावा देने के लिए छत्रप (कुकुरमुत्ते की भाँति प्रकट हो रहा है। निराशाजनक फूट तथा असामंजस्य का सर्वत्र ही बोलबाला है। विभिन्न सम्प्रदायों में संघर्ष चल रहा है। सर्वत्र ही मतभेद, फूट, न्यायालयों में बाद, झड़पें, मुठभेड़ तथा पिशुनता का प्राबल्य है। न तो शान्ति है और न मेल-मिलाप। एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के शिष्यों से सड़कों और चौराहों पर लड़ते-फिरते हैं।
धूर्त योगी तथा ढोंगी गुरु
एक नवयुवक हारमोनियम का प्रशिक्षण तथा स्वल्प वक्तृत्व-शक्ति प्राप्त कर मंच पर चढ़ता है। कुछ ही वर्षों में आचार्य अथवा गुरु होने का ढोंग रचता है, कुछ अण्ड-बण्ड प्रपत्र तथा गाने प्रकाशित करता है और अपना एक अलग सम्प्रदाय स्थापित कर बैठता है। भारत में अभी भी गम्भीर मूर्खताओं का प्राचुर्य है, जहाँ कोई भी व्यक्ति अल्पावधि में अपने अनुयायी बना सकता है।
आसनों, बन्धों तथा प्राणायामों का थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त अन्य नवयुवक गुप्त रूप से रखे हुए चालीस दिन तक पर्याप्त होने वाले खाद्य-पदार्थ वाले एक भूमिगत कक्ष में अपने को बन्द कर लेता है। वह कुछ जड़ी-बूटी खा लेता है जो कुछ दिनों के लिए क्षुधा तथा पिपासा को नष्ट कर देती है। भगवान् ही जानता है कि वह कक्ष में क्या करता है। वह कक्ष में सोता है। तत्पश्चात् वह मिथ्या समाधि से बाहर आता है। यह तितिक्षा का अल्प अभ्यास मात्र है। उसके संस्कार तथा वासनाएँ किंचित् भी नष्ट नहीं होतीं। वह पहले का ही सांसारिक व्यक्ति है। वह धन-संग्रह करने तथा शिष्य बनाने के लिए इधर-उधर मारा-मारा फिरता है। वह योगी - गुरु होने का ढोंग रचता है। अज्ञानी सांसारिक जन सहज में ही प्रवंचित होते हैं। दुःखद बात तो यह है कि लोग इस प्रकार अनुत्तरदायी ढोंग रचने वाले नवयुवकों के मूर्खतापूर्ण कार्यों के कारण वास्तविक समाधि में प्रवेश करने वाले सच्चे योगियों में भी श्रद्धा खो बैठते हैं। इन नवयुवकों ने योग तथा आध्यात्मिक जीवन के गुरुत्व को नहीं समझा है। निःसन्देह समाधि सार्वजनिक सड़कों पर प्रदर्शनार्थ नहीं है। समाधि एक पवित्र कार्य है। समाधि इन्द्रजाल नहीं है। यह व्यवहार संक्रामक हो चला है। अनेक नवयुवकों ने यह प्रदर्शन अथवा करतूत आरम्भ कर दी है।
इन धूर्त योगियों, दिन-दहाड़े प्रवंचना करने वालों, ढोंगी गुरुओं, कुल-कलंकों से सावधान रहें जो संसर्गज परजीवी तथा समाज पर भार हैं; जो देश के लिए संकट तथा अनभिज्ञ और भोले-भाले लोगों की सम्पत्ति खसोटने वाले गृध्र हैं।
कुछ लोग वृद्धावस्था में अपनी सेवा के लिए शिष्य बनाते हैं। वे अपने शिष्यों की चिन्ता नहीं करते।
महिलाओं को चेतावनी
तथाकथित गुरुओं और आचार्यों से महिलाएँ सहज ही प्रवंचित हो जाती हैं। महिलाएँ बहुत ही सरल स्वभाव तथा आशु विश्वासी होती हैं। वे मधुर संगीत तथा स्वर-माधुर्य से बड़ी ही सरलता से आकर्षित हो जाती हैं। श्रुतिमधुर ध्वनि की सहज ही शिकार बनती हैं। ये गुरु नारी जाति की गोष्ठियों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। वे उन्हें सहज ही प्रभावित कर लेते हैं और निरायास उनका शोषण करते हैं। वे उन्हें अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बना लेते हैं। वे उनसे अनुचित लाभ उठाते हैं, अपनी उदर-पूर्ति करते हैं तथा कौशेय वस्त्र और विशेष प्रकार के जूते धारण कर घूमते-फिरते हैं। गृहस्थों के लिए महिला शिष्याएँ बनाना शास्त्र-सम्मत नहीं है। जो लोग शालीन जीविकोपार्जन के लिए महिला शिष्याएँ बनाते हैं, वे विष्ठा में प्रमोद करने वाले कीट के सदृश हैं। ऐसे दम्भी लोगों के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। वे रौरव तथा महारौरव नरक में निर्ममतापूर्वक डाल दिये जाते हैं।
हे देवियो! अब जाग जायें। अपने नेत्र खोलें। अब आप सब शिक्षित हो चली हैं। अपने विवेक का उपयोग करें। केवल प्रवचनों तथा संगीत से प्रभावित न हो जायें। आडम्बरी गुरुओं से सावधान रहें। गृहस्थ को कदापि अपना गुरु न बनायें। उससे कभी दीक्षा न लें। यदि आप ऐसा करेंगी, तो आप रोयेंगी तथा दुष्परिणाम भोगेंगी। जिस व्यक्ति को आप अपना गुरु वरण अनुकरणीय होना चाहिए। उसे काम से मुक्त होना चाहिए। उसे सभी प्रकार के हो चाहिए। ह -शाखों का ज्ञाता होना चाहिए। आपको बनाने पर आपका मार्ग-दर्शन करने के अन्तः- आध्यात्मिक शक्ति तथा आत्म-साक्षात्कार से सम्पन्न होना चाहिए।
पति को चाहिए कि उसकी पत्नी जिस व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहती है, उसकी उचित संवीक्षा अथवा सम्यक् परीक्षण और परिचय के बिया उसे अपना गुरु बनाने की अनुमति न दे। यदि वे गुरु बनाने को वास्तव दे अधिक महत्त्व देते हैं, व्यक्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन तथा जाँच-पड़ताल के पश्चात् तथा उसके साथ सुदीर्घ काल तक रहने के अनन्तर ही उसे अपना गुरु वरण करें। पति और पत्नी के पृथक् पृथक् गुरु नहीं होने चाहिए, अन्यथा संघर्ष उठ खड़ा होता है। उनका उभयनिष्ठ गुरु होना चाहिए।
सम्प्रदायों तथा पन्थों की विभीषिका
चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, स्वामी दयानन्द —ये सभी उदारमना, उदात्त आत्माएँ थीं। उनकी सभी शिक्षाएँ उदात्त तथा विश्वजनीन थीं। उन्होंने कभी भी अपना पन्थ अथवा सम्प्रदाय स्थापित करना नहीं चाहा। यदि वे आज जीवित होते, तो वे अपने अनुयायियों की करतूतों पर अश्रुपात करते। अनुयायी ही गम्भीर भूलें तथा प्रमाद करते हैं। उनमें विशाल हृदय का विकास नहीं हुआ होता है। वे संकीर्णमना होते हैं। वे मतभेद, दलगत भावना तथा सभी प्रकार के उपद्रव उत्पन्न करते हैं।
धर्माचायों को कभी भी अपना सम्प्रदाय स्थापित नहीं करना चाहिए। उनमें व्यापक अन्तर्दृष्टि होनी चाहिए। सम्प्रदाय की स्थापना करने का अर्थ है विश्व शान्ति को भंग करने वाले एक युद्ध-केन्द्र का निर्माण। वह देश का हित करने की अपेक्षा हानि ही अधिक करता है। उसकी एक संस्था हो सकती है, जिसके सिद्धान्त तथा वाद उदार और सार्वजनीन, दूसरे धर्मों के सिद्धान्तों तथा वादों के अविरोधी और सर्वतः सभी द्वारा स्वीकार्य तथा अनुकरणीय हों।
सद्गुरु के लक्षण
सद्गुरु के ये लक्षण हैं। यदि आप किसी व्यक्ति में इन लक्षणों को पाते हैं, तो आप तत्काल उसे अपना गुरु स्वीकार कर लें। सच्चा गुरु वह है जो ब्रह्मनिष्ठ तथा श्रोत्रिय हो। उसे आत्मा तथा वेदों का पूर्ण ज्ञान होता है। वह साधकों की शंकाओं का निवारण कर सकता है। उसमें समदृष्टि तथा सन्तुलित मन होता है । वह राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि से मुक्त होता है। वह करुणा-सागर होता है। उसकी उपस्थिति मात्र से व्यक्ति को शान्ति तथा मनोत्कर्ष की प्राप्ति होती है। उसकी उपस्थिति में साधक की सभी शंकाएँ विदूरित हो जाती हैं। वह किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। वह उल्लास तथा आनन्द से परिपूर्ण होता है। वह सच्चे साधकों की खोज में रहता है।
गुरु के चरण-कमलों को नमस्कार! मुझे सच्चे' गुरु में पूर्ण विश्वास है। मेरे लिए गुरु परम आराध्य हैं। मेरा हृदय उनके चरण-कमलों की सदा सेवा करने के लिए लालायित रहता है। मेरा विश्वास है कि मन के मलों का निवारण करने के लिए गुरु की सेवा से अधिक पावनकारी अन्य कुछ भी नहीं है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि दूसरे तट अमरत्व तक ले जाने के लिए गुरु की संगति ही एकमात्र सुरक्षित नौका है।
व्यापारिक गुरुपन
किन्तु मैं व्यापारिक गुरुपन को नापसन्द करता हूँ। मुझे उन पाखण्डियों के व्यवहार पर घोर अप्रसन्नता होती है जो गुरु तथा आचार्य होने का ढोंग करते हैं और शिष्य बनाते हैं तथा धन आहरण करते. घूमते-फिरते हैं। इस विषय में आप सभी मुझसे सहमत होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वे समाज के कण्टक है। गुरुपन केवल व्यवसाय बन गया है। इसका भारत की भूमि से पूर्णतया उन्मूलन करना चाहिए। यह भारतवासियों का बहुत ही विनाश तथा अहित कर रहा है। यह पाश्चात्य देशवासियों तथा विभिन्न देशों के लोगों के मन पर बहुत ही बुरा प्रभाव रहा है। भारत अपने इस गुरुपन के व्यवहार के कारण अपनी आध्यात्मिक गरिमा खो रहा है। इस गम्भीर व्याधि का दमन करने तथा इसे आमूल नष्ट करने के लिए तत्काल सशक्त पग उठाने चाहिए। इसका उन्मूलन करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए। इसने विकराल रूप धारण कर लिया है। यह बहुत ही संक्रामक हो चला है। अनेक लोगों ने इस गुरुपन-व्यवसाय को शालीन जीविका के एक सरल साधन के रूप में अपनाया है। बेचारे अनभिज्ञ महिलाएँ तथा पुरुषों का इन छद्म गुरुओं द्वारा बड़े पैमाने पर शोषण होता है। क्या ही लज्जास्पद विषय है!
अनेक गुरु इधर-उधर घूमते-फिरते हैं। वे प्रवचन करते तथा भाषण देते हैं। उन्हें ब्रह्मसूत्र तथा गीता कण्ठस्थ होते हैं; किन्तु उनमें ज्ञान-ध्यान नहीं होते हैं। वे सहज ही उत्तेजित हो उठते हैं। उनका अभिमान बहुत दृढ़ होता है। उनमें दैवी गुणों तथा साधुत्व का अभाव होता है। उनमें सेवा-भाव नहीं होता है। वे सेवा, कीर्तन आदि की निन्दा करते हैं। वे बहुत से लोगों को भुजाओं से पकड़ लेते हैं। वे उनकी पीठ पर हाथ रख कर आशीर्वाद देते हैं; किन्तु वे एक भी व्यक्ति को मोक्ष तक नहीं पहुँचा सकते।
जनता किसी को तभी अपना गुरु स्वीकार करती है, यदि वह कुछ सिद्धियाँ प्रदर्शित करे। यह गम्भीर भूल है। उन्हें अति आशु विश्वासी नहीं होना चाहिए। वे इन कपटी योगियों से सहज ही प्रवंचित होंगे। उन्हें अपने विवेक तथा तर्कणा-शक्ति का उपयोग करना चाहिए। उन्हें किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व गुरु की विधियों, आदतों, प्रकृति, आचरण, वृत्ति, स्वभाव आदि का अध्ययन करना चाहिए और उसके शास्त्र- ज्ञान की जाँच करनी चाहिए।
इस देश की जनता को पथ-भ्रष्ट करने तथा लूटने वाले इन कुल-कलंक लोगों के पास जाने के स्थान पर भगवान् कृष्ण, भगवान् राम, भगवान् शिव, अपने अन्तर्यामी प्रभु को अपना गुरु मानना तथा उनके मन्त्र का जप करना श्रेयस्कर है।
गौरवशाली भारत श्री शंकर अथवा श्री दत्तात्रेय जैसे सच्चे गुरुओं से भरपूर हो! वह इन छद्म गुरुओं तथा गुरुपन से मुक्त हो जो कि महा अभिशाप है! सनातन-धर्म के विश्वजनीन सिद्धान्त विश्व में फूलें-फलें ! धर्माचार्य विविध पन्थों तथा सम्प्रदायों के एकीकरण के लिए यथाशक्य प्रयास करें। वे नये सम्प्रदायों की स्थापना न करें। यह साम्प्रदायिक लड़ाई-झगड़े तथा कलह सदा के लिए समाप्त हो जायें! यह देश त्याग, संन्यास तथा आत्म-साक्षात्कार का लक्ष्य रखने वाले सन्त-महात्माओं, योगियों, भक्तों तथा संन्यासियों का देश होने की अपनी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को सदा बनाये रखे! एकता, शान्ति तथा सामंजस्य संसार-भर में अभिभावी हों! हम सब पर गुरुओं का आशीर्वाद रहे ! वे अध्यात्म-पथ पर हमारा मार्ग-दर्शन करें!
अष्टम अध्याय
संन्यासियों से वार्ता
आपातवैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धिपारं प्रतियातुमुद्यतान् ।
आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले विगृह्य कण्ठे विनिवर्त्य वेगात् ।।
"संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा - रूपी ग्राह अतिवेग से बीच में ही रोक कर गला पकड़ कर डुबो देता है।"
(विवेक-चूड़ामणि : ८१)
हरि ॐ ! ब्रह्म को मेरी श्रद्धांजलि। श्री शंकराचार्य, महापुरुषों तथा संन्यासियों को नमस्कार!
संन्यासी वह है जिसने देहाध्यास (देह-भावना), स्वार्थपरता, वासनाओं, अहंभाव तथा अभिमान का न्यास (त्याग) कर दिया है। ब्रह्मा के चार कुमार (श्री सनक, सनन्दन, सनत्कुमार तथा सनत्सुजात), श्री दत्तात्रेय तथा श्री शंकराचार्य इस विशुद्ध निवृत्ति-मार्ग के पुरोगामी थे। वे इस संन्यास आश्रम के प्रवर्तक हैं।
काल-प्रवाह
संसार आर्थिक, प्रजातीय, सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ आध्यात्मिक प्रगति भी चाहता है। आध्यात्मिक पक्ष की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वही आधार है। वही चरम लक्ष्य है। आजकल कर्मयोग-क्षेत्र के नेता गण केवल कर्म पर ही बल देते हैं। उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष की पूर्णतया उपेक्षा कर रखी है। अनेक संस्थाओं के संन्यासी भी केवल सामाजिक सेवा कर रहे हैं। कुछ संन्यासियों में केवल पण्डितोचित विद्वत्ता होती है। वे कुछ समय तक थोड़े-से सम्मान के अधिकारी होते हैं। उन्होंने भी जीवन के चिन्तनशील पक्ष को अलग फेंक दिया है। वे जनता के मन पर वास्तविक तथा चिरस्थायी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं; क्योंकि उनके पृष्ठाधान में यथार्थ आध्यात्मिक सामग्री अथवा आन्तरिक आत्मिक बल नहीं होता।
आध्यात्मिक व्यक्तियों, योगियों, ज्ञानियों तथा संन्यासियों को धूमकेतु, कार्तिक माह की द्वितीया के चन्द्रमा अथवा प्रभु यीशु की भाँति विश्व मंच पर अल्प काल के लिए उपस्थित होना चाहिए। उन्हें अपनी शक्ति प्रवाहित करनी चाहिए, विशाल कर्म सम्पन्न करना चाहिए और फिर कर्मक्षेत्र से अदृश्य हो जाना चाहिए। अधिक समय तक आध्यात्मिक वर्गों का संचालन करने तथा आश्रम खोलने का कार्य कनिष्ठ संन्यासियों का है। यह प्रचण्ड असाधारण आध्यात्मिक गुणों वाले व्यक्ति की प्रकृति के उपयुक्त नहीं होता है। वे अल्प काल में ही वसुन्धरा को वैसे ही आध्यात्मिक जल अथवा अमरत्व प्रदायक अमृत (दिव्य ज्ञान) से आप्लावित कर देते हैं जैसे प्रावृट काल के चार महीनों में गंगा कर देती है।
सुखद जीवन-यापन का प्रलोभन
किसी संन्यासी अथवा गृहस्थ को सुखी जीवन-यापन हेतु आश्रम नहीं खोलना चाहिए। अनेक संन्यासी जब वे आश्रम खोलते हैं तो प्रारम्भ में, मेरे कहने का भाव यह है कि जब वे निर्धन होते हैं, तब वे निर्दोष होते हैं; किन्तु जब वे धनवान हो जाते हैं, जब उनके बहुत से प्रशंसक तथा भक्त बन जाते हैं, तब उनकी निःस्वार्थ सेवा की भावना क्षीण पड़ जाती है और उनके हृदय में उसका स्थान स्वार्थपरायण उद्देश्य ले लेता है। जिस उद्देश्य से उन्होंने आश्रम खोले, वह विफल हो जाता है। तब वह धनोपार्जन की संस्था बन जाती है। लोगों को उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। यदि संस्था का प्रमुख व्यक्ति वैराग्य तथा परम त्यागमय जीवन-यापन करता है। तो आश्रम शाश्वत शान्ति, आनन्द तथा सुख का केन्द्र अथवा नाभिक बन जाता है। यह लाखों लोगों को आकर्षित करता है। संसार को सदा ही ऐसे आश्रमों की आवश्यकता रहती है, जिनके प्रमुख ऐसे असाधारण आध्यात्मिक गुणों वाले व्यक्ति हों ।
कुछ युवक संन्यासी कुचला के बीज का सेवन करते हैं, दो वर्ष में एक सौ बीस बीज निगल जाते हैं, तीन वर्षों तक लघु सिद्धान्त कौमुदी तथा न्याय का अध्ययन करते हैं, कल्पना करते हैं कि वे सच्चे सिद्ध बन गये हैं और सांसारिक व्यक्तियों से स्वच्छन्द रूप से मिलते हैं। यह भयंकर भूल है। कुचला से नपुंसकता उत्पन्न होती है। नपुंसकता ब्रह्मचर्य में संस्थित होना नहीं है। यह मानी हुई बात है कि उनका शीघ्र पतन होता है। पूर्ण ज्ञानियों तथा पूर्ण विकसित योगियों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्हें सांसारिक व्यक्तियों के साथ अन्धाधुन्ध, स्वच्छन्द रूप से मिलने-जुलने का परिहार करना चाहिए। मत्स्य के युग्मन के दृश्य ने एक विकसित ऋषि को उद्दीप्त कर दिया। एक महिला के कंकणों की झनकार, किनारीदार अथवा रंगीन वस्त्र भी मन में तीव्र उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। उनके अपने दूषित साहचर्य होते हैं। काम-वासना बहुत ही शक्तिशालिनी है। माया रहस्यमयी है। हे साधको! सावधान रहो ।
जिह्वा तथा स्वादेन्द्रिय अनुशासनहीन युवक साधकों, ब्रह्मचारियों तथा संन्यासियों को सत्संग कराने के बहाने गृहस्थों के निकट सम्पर्क में आने को बाध्य करती हैं। हे साधको! क्या तुमने अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के लिए ही अपने माता-पिता को छोड़ा, अपने पद और सम्पत्ति का त्याग किया तथा संन्यास ग्रहण किया है? अथवा ऐसा तुमने आत्म-साक्षात्कार करने के लिए किया है? यदि तुमने पूर्वोक्त के लिए ऐसा किया है, तो तुम संसार में धनोर्पाजन कर इसे भली प्रकार कर सकते थे। संन्यास आश्रम को कलंकित न करो। यदि जिह्वा अनियन्त्रणीय है तो गैरिक वस्त्र उतार दो, संसार में वापस चले जाओ, कुछ कार्य करो और धनोर्पाजन करो। कर्मयोग के द्वारा अपना उद्विकास करो। जिह्वा के संयम के अभाव में मन का संयम सम्भव नहीं है।
क्या यह सत्संग है ?
आजकल सत्संग विकृत हो चला है। एक प्रकार के मनोरंजन अथवा मनोविनोद के रूप में इसका ह्रास हो गया है। सायंकाल में एक घण्टे तक संन्यासियों और गृहस्थों के मध्य कुछ निरर्थक सांसारिक चर्चा, कुछ राजनीति, कुछ निन्दा तथा पैशुन्य, कुछ मूर्खतापूर्ण ही - ही तथा ठहाकों और अस्पष्ट सामान्योक्ति में कोमल भावुकतापूर्ण उद्गारों के मिश्रण के साथ वेदान्त की गपशप को ही सत्संग का नाम दिया जाता है। सत्संग कराने वाले संन्यासियों तथा श्रोताओं का मन अनेक वर्षों तक की सत्संग-माला के अनन्तर भी वैसा ही रहता है। कोई भी उत्थान और आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है।
साधुओं तथा संन्यासियों को संसार में विचरण करते समय गृहस्थों के समक्ष अनुकरणीय वैराग्यमय जीवन प्रदर्शित करना चाहिए। उन्हें गृहस्थों से जीवन की केवल अत्यावश्यक वस्तुएँ ही ग्रहण करनी चाहिए। उन्हें उनके साथ बहुत स्वच्छन्दतापूर्वक नहीं मिलना-जुलना चाहिए। उन्हें ग्राम अथवा नगर के बाहर एकान्त स्थान में निवास करना चाहिए। उन्हें आध्यात्मिक वर्ग गम्भीर ढंग से चलाना चाहिए। मध्यावधि में उन्हें सांसारिक विषयों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्हें हँसी लाने के लिए बहुत अधिक कहानियों का सन्निवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें हास-परिहास नहीं करना चाहिए। गम्भीर प्रशान्ति रहनी चाहिए। सभी स्रोता मन्त्र-मुग्ध-से होने चाहिए। वहाँ पूर्ण नीरवता होनी चाहिए। केवल तभी गृहस्थ जनों पर प्रभाव पड़ेगा। उन्हें • अनुभव होगा कि सत्संग से उन्हें कुछ प्राप्त हुआ है।
खीर-परौठा पक्षी
जिस समय संन्यासी गृहस्थों से बारम्बार अनेक वस्तुओं की माँग करने लगता है, तो वह अपना सम्मान एवं प्रभाव खो बैठता है। वह उस स्थान को तुरन्त छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। कुछ निर्लज्ज संन्यासी लगातार कई महीनों तक गृहस्थों के मध्य परजीवी बने टिके रहते हैं। वे खीर-परौठा पक्षी हैं। वे सच्चे संन्यासी नहीं हैं। अधिकारियों को आगामी जनगणना के समय अपना विवरण अग्रेषित करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। इन व्यक्तियों का नाम साधु और संन्यासियों की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। मेमने की खाल में भेड़िये की भाँति वे रंगीन वस्त्रों में व्यावसायिक भिखमंगे हैं। सच्चे संन्यासियों का ठीक अभिलेख होना चाहिए। साधुओं की संख्या को बढ़ाने और साधुओं की संख्या ७४ लाख दर्शाने से क्या लाभ है? तुम्हें २००० से अधिक अच्छे सांस्कृतिक संन्यासी नहीं मिलेंगे जो अपने तथा सामान्य रूप से देश के लिए उपयोगी हों। एक सच्चा साधु या संन्यासी तेजस्वी सूर्य की भाँति है। वह अहर्निश देदीप्यमान रहता है।
साधकों का प्रशिक्षण
साधुओं तथा संन्यासियों के लिए एकमात्र ऋषिकेश ही सर्वोत्तम स्थान है । यहाँ निःशुल्क भोजन, निःशुल्क कुटीर तथा निःशुल्क पर्णशालाएँ उपलब्ध हैं। एक सुन्दर पुस्तकालय है। चिकित्सा-सहायता मिल सकती है। तुम पक्षी की भाँति स्वतन्त्र रह सकते हो। तब तुम यत्र-तत्र क्यों भटक फिरते हो? यदि एक साधु-संन्यासी अथवा साधक वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति तथा आत्म-साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसे न्यूनातिन्यून बारह वर्ष तक एक दिन के लिए भी बाहर न जा कर इस स्थान में टिके रहना चाहिए और कठोर तथा अविच्छिन्न साधना करनी चाहिए। स्थान- परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा तथा हिमालय नित्य प्रेरणादायी, उत्थानकारी तथा स्वास्थ्यप्रद हैं। स्थान-परिवर्तन निर्बल संकल्प वाले व्यक्तियों, भ्रान्त चिकित्सकों तथा धनी लोगों की मूर्खतापूर्ण कल्पना है।
एक संन्यासी अथवा साधु स्थान-स्थान पर घूम-फिर कर मंचों पर व्याख्यान देने से कहीं अधिक ठोस तथा फलोत्पादक कार्य अपने कुटीर की देहली पर ही कर सकता है। जब पुष्प प्रस्फुटित होता है, तब वह मधु मक्खियों को निमन्त्रण नहीं भेजता है। मधुमक्खियाँ स्वयं ही आती हैं। इसी भाँति सत्य के सच्चे जिज्ञासु सच्चे संन्यासियों को उनके द्वार पर ही चतुर्दिक् से घेरे रहते हैं। संन्यासियों को इधर-उधर जाने की तथा विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है। मंच के भाषणों में केवल आधे घण्टे की अस्थायी उत्तेजना होती है। कुछ कोनों में कुछ हो-हल्ला, कुछ संघर्ष, कुछ कलह, करतल ध्वनि, साधु-साधु के शब्द होते हैं। संन्यासियों के कुटीरों में सच्चे अधिकारी ही उनसे मिलने जायेंगे। इन साधकों के हृदय संन्यासियों के उपदेश मे वास्तव में बेधे जा सकते हैं। साधकों को प्रशिक्षण देना महत्तम सेवा है जो संन्यासी कर सकता है। प्रत्येक साधक आध्यात्मिक केन्द्र अथवा आनन्द, शान्ति और ज्ञान विकीर्ण करने अथवा प्रसारित करने वाला केन्द्र बन जाता है। जब संन्यासी घूमता है, तो उसका समय नष्ट होता है। कुतूहलवश सभी प्रकार के लोग उससे मिलने आते हैं। आजकल गृहस्थ लोग उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वे नितान्त स्वार्थी हो गये हैं। 'स्वामी जी महाराज! मेरे लायक कुछ सेवा बताइए' ऐसा कह कर वे कुछ दिखावटी सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। यह निरा धोखा, पाखण्ड और धूर्तता है।
जब कोई व्यक्ति गैरिक वस्त्र धारण करता है, तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसने महान् संन्यास आश्रम में प्रवेश किया है तथा उसके कन्धों - पर महान् उत्तरदायित्व आ पड़ा है और वह शीघ्र ही विश्व का धार्मिक तथा आध्यात्मिक गुरु बनने जा रहा है। उसे सभी अभिजात, दिव्य गुणों से सम्पन्न बनने तथा शुद्धता और वैराग्यमय आदर्श जीवन यापन करने का यथासम्भव प्रयास करना चाहिए।
सच्चे संन्यासी संसार के लिए प्रकाश स्तम्भ और पथ-प्रदर्शक हैं। जैसे प्रकाश-गृह सुदूर सागर में स्थित जलपोतों को प्रकाश प्रेषित करता है, वैसे ही संन्यासी भी अज्ञान तथा अन्धकार के पंक में निमज्जित दूर देश के लोगों में अपना दिव्य प्रकाश विकीर्ण करते हैं। वे सारे संसार को प्रभावित कर सकते हैं।
सच्चे संन्यासियों की जय हो जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है, जो सन्मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं! उन संन्यासियों को अभिवादन है जो निज-स्वरूप में स्थित हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं! परिव्राजकाचार्यों की, ब्रह्मविद्या के गुरुओं की जय हो जो चतुर्दिक् आत्मज्ञान का प्रसार कर रहे हैं! उनका आशीर्वाद हम सब पर हो !
नवम अध्याय
गुरु-भक्ति-योग
जिस प्रकार आशु भगवद्-दर्शन के लिए कीर्तन-साधना कलियुग की विशेष साधना बन गयी है, उसी प्रकार इसमें आपके लिए एक नया योग, ऐसा योग दिया जा रहा है जो इस सन्देह तथा अविश्वास के, अभिमान तथा अहं के युग में सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप से उपयुक्त है। यह गुरु-भक्ति-योग है। यह योग चमत्कारिक है। इसकी शक्ति अत्यधिक विशाल है। इसकी प्रभावोत्पादकता सर्वाधिक अमोघ है। गुरु-भक्ति-योग की महिमा अवर्णनीय है। यह इस युग के लिए सर्वोत्कृष्ट योग है। इससे भगवान् यहाँ आपके समक्ष सशरीर प्रकट होते और इस जीवन में ही आपके साथ चलते-फिरते हैं। कठोर राजसिक अहं साधक का कट्टर शत्रु है। गुरु-भक्ति-योग दर्प को नष्ट करने तथा दुष्ट अहं को विगलित करने के लिए एक सर्वाधिक निश्चित तथा सर्वोत्कृष्ट साधना है। जिस प्रकार एक विशेष प्रकार के घातक जीवाणु का एक विशेष प्रकार की रासायनिक जीवाणुनाशी औषधि से ही विनाश किया जा सकता है, उसी प्रकार अविद्या तथा अहंकार को नष्ट करने के लिए यह अनुपम गुरु-भक्ति-योग एक अद्वितीय औषधि है। यह एक सर्वाधिक उग्र 'मायानाशक' तथा 'अहंनाशक' है। वे सर्वथा शक्ति हीन हो जाते हैं और उस भाग्यशाली आत्मा को जिसने गुरु-भक्ति-योग की भावनाओं से अपने को सन्तृप्त कर लिया है अब पूर्ववत् आक्रान्त नहीं करते। वह व्यक्ति वास्तव में ही धन्य है जो इस योग को रुचिपूर्वक अपनाता है; क्योंकि उसे अन्य सभी योगों में सर्वोच्च सफलता प्राप्त होगी। उसे कर्म, भक्ति, ध्यान तथा ज्ञान योगों की पूर्णता के साथ श्रेष्ठतम फल उपलब्ध होंगे।
इस योग का अधिकारी बनने के लिए सत्यशीलता, श्रद्धा तथा आज्ञाकारिता का सरल त्रिक है। पूर्णता की अपनी अभीप्सा में सत्यशील रहें। अनिश्चित तथा निरुत्साह न रहें। आपने जिसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, उसमें पूर्ण श्रद्धा रखें। सन्देह की छाया भी आपके पास न फटकने पाये। जब आपने उसमें एक बार पूर्ण विश्वास रखा है, तो समझ लें कि वह आपको जो कुछ भी आदेश देता है, निश्चय ही आपके सर्वोत्तम हित में होगा। उसके उपदेशों का अक्षरशः पालन करें। इस प्रकार कार्य करने में आप सत्यशील रहें और मेरे इस कथन को स्वीकार करें कि आप पूर्णता प्राप्त करेंगे। मैं आपको बलपूर्वक आश्वासन देता हूँ।
अब गुरु-भक्ति-योग का विवेचन किया जाता है।
( १) गुरु-भक्ति-योग सद्गुरु को पूर्ण आत्म-निवेदन करना है।
(२) गुरु-भक्ति-योग के आठ महत्त्वपूर्ण अंग इस प्रकार हैं—(क) गुरु-भक्ति के अभ्यास के लिए वास्तविक स्थायी आकांक्षा; (ख) सद्गुरु के विचार, वाणी तथा कर्म में पूर्ण श्रद्धा; (ग) गुरु को नम्रतापूर्वक साष्टांग नमस्कार करना तथा उनके नाम का जप करना; (घ) गुरु के आदेशों के पालन में पूर्ण आज्ञाकारिता; (ङ) फल-प्राप्ति की आशा रखे बिना सद्गुरु की वैयक्तिक सेवा करना; (च) सद्गुरु के चरण-कमलों की भाव तथा भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करना; (छ) सद्गुरु के दिव्य कार्य हेतु आत्म-समर्पण अथवा तन-मन-धन अर्पण करना; तथा (ज) सद्गुरु की सौम्य कृपा केप्राप्त्यर्थ उनके पवित्र चरणों का ध्यान तथा उनके उपदेशों का श्रवण तथा उनका सच्चाईपूर्वक अभ्यास ।
(३) गुरु-भक्ति-योग स्वयं में एक योग है।
(४) यदि साधक गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास नहीं करता, तो उसके लिए भगवान् के साथ योग कराने वाले अध्यात्म-पथ में प्रवेश करना सम्भव नहीं है।
(५) जिसे गुरु-भक्ति-योग-दर्शन-प्रणाली का ज्ञान है, वहीं अपने गुरु को अप्रतिबन्ध रूप से समर्पण कर सकता है।
(६) जीवन के परम लक्ष्य अर्थात् आत्म-साक्षात्कार की प्राप्ति गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास से होती है।
(७) गुरु-भक्ति-योग एक वास्तविक सुरक्षित योग है, जिसका अभ्यास निरापद रूप से किया जा सकता है।
(८) गुरु-भक्ति-योग का सार गुरु के आदेशों के पूर्णतः पालन तथा उनके उपदेशों को जीवन में कार्य रूप में परिणत करने में है।
(९) गुरु-भक्ति-योग का उद्देश्य गुरु के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण द्वारा व्यक्ति को विषय-पदार्थों की दासता तथा प्रकृति के पाश मुक्त से कराना तथा उसे अपने परम मुक्त-स्वरूप का अनुभव कराना है।
(१०) जो गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास करता है, वह अहं का निरायास ही उन्मूलन कर सकता है और संसार रूपी दलदल को सहज ही पार कर सकता है।
(११) जो गुरु-भक्ति-योग का पूर्ण हृदय के साथ नियमित रूप से अभ्यास करता है, उसे वह अमरत्व तथा शाश्वत सुख प्रदान करता है।
(१२) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास मन को शान्ति तथा सन्तुलन प्रदान करता है।
(१३) गुरु-भक्ति-योग स्वर्गिक सुख के साम्राज्य का द्वार खोलने की सर्वकुंजी (मास्टर - की) है।
(१४) जीवन का लक्ष्य गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास द्वारा सद्गुरु की कल्याणमयी कृपा प्राप्त करना है।
(१५) सद्गुरु के पूज्य चरणों के पास नम्रतापूर्वक जायें। सद्गुरु के प्राण-रक्षक चरणों में साष्टांग प्रणाम करें। सद्गुरु के चरण-कमलों की शरण लें। सद्गुरु के पावन चरणों की पूजा करें। सद्गुरु के पावनकारी चरणों में बहुमूल्य उपहार भेंट करें। सद्गुरु के महिमामय चरणों की सेवा में जीवन अर्पण करें। यही गुरु-भक्ति-योग का रहस्य है।
(१६) सद्गुरु के पावन चरणों में आत्म-समर्पण करना ही गुरु-भक्ति-योग का आधार है।
(१७) आपसे गुरु-भक्ति-योग में मात्र गम्भीर तथा सच्चे प्रयास की अपेक्षा की जाती है।
(१८) गुरु-भक्ति-योग में गुरु के प्रति भक्ति सर्वोत्कृष्ट तत्त्व है।
(१९) गुरु में श्रद्धा गुरु-भक्ति-योग-रूपी निश्रयणी का प्रथम सोपान है।
(२०) श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के विचार, वाणी तथा कार्य में पूर्ण विश्वास गुरु-भक्ति-योग का सार है।
(२१) इस युग में सर्वोत्कृष्ट तथा सरलतम योग-साधना गुरु-भक्ति-योग है।
(२२) गुरु-भक्ति-योग-दर्शन में महत्तम सूत्र गुरु का परब्रह्म के साथ तादात्म्य करना है।
(२३) गुरु-भक्ति-योग-दर्शन का व्यावहारिक रूप गुरु को अपने इष्टदेव से अभिन्न समझना है।
(२४) गुरु-भक्ति-योग कोई दर्शन नहीं है, जिसका ज्ञान व्याख्यानों अथवा पत्र-व्यवहार द्वारा प्रदान किया जा सके। शिष्य को गुरु के पास अनेक वर्षों तक गुरु के सान्निध्य में रहना चाहिए तथा आत्म-संयम, अनुशासन तथा ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन-यापन करते हुए गम्भीर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।
(२५) गुरु-भक्ति-योग समस्त विज्ञानों का विज्ञान है।
(२६) गुरु-भक्ति-योग अमरत्व, शाश्वत सुख, मुक्ति, पूर्णता, अक्षुण्ण आनन्द तथा चिरन्तन शान्ति प्रदान करता है।
(२७) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास सांसारिक पदार्थों के प्रति अनासक्ति तथा वैराग्य उत्पन्न करता और कैवल्य मोक्ष प्रदान करता है।
(२८) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास मनोविकारों तथा आवेगों के नियन्त्रण में शिष्य के लिए सहायक होता है, प्रलोभनों का सामना करने तथा मन से क्षुब्धकारी तत्त्वों को विदूरित करने की शक्ति प्रदान करता है तथा अन्धकार के दूसरे तट पर ले जाने वाली गुरु कृपा की प्राप्ति का अधिकारी बनाता है।
(२९) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास अमरता, परम शान्ति तथा नित्य आनन्द प्रदान करता है।
(३०) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास आपको भय, अज्ञान, निराशा, किंकर्तव्यविमूढ़ता, रोग तथा चिन्ता से मुक्त होने में समर्थ बनाता है।
(३१) गुरु-भक्ति-योग वैयक्तिक भावना, इच्छा, समझ तथा निश्चय के ऊर्ध्वकरण द्वारा अहंभाव का असीम चेतना में रूपान्तरण है।
(३२) गुरु-भक्ति-योग में प्रस्तुत साधनाएँ दूसरे तट, निर्भयता तक ले जाने के लिए बहुत ही सरल तथा अमोघ उपाय हैं।
(३३) गुरु-भक्ति- योग गुरु कृपा द्वारा प्राप्त कठोर अनुशासन का पथ है।
(३४) गुरु-भक्ति-योग के दर्शन के अनुसार फलाशा-रहित गुरु-सेवा तथा गुरु के चरण-कमलों की उत्तरोत्तर वर्धमान भक्ति समग्र साधना है।
(३५) जो कोई नैतिक पूर्णता, गुरु-भक्ति आदि के बिना ही गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास करता है, उसे गुरु कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है।
(३६) गुरु-भक्ति-योग अन्य सब योगों—यथा कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग, हठयोग आदिका आधार है।
(३७) जो व्यक्ति गुरु-भक्ति-योग से विमुख है वह मृत्यु, अन्धकार तथा अज्ञान की परम्परा को प्राप्त होता है।
(३८) गुरु-भक्ति-योग की साधना जीवन के परम ध्येय की प्राप्ति का निश्चित पथ बतलाती है।
(३९) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास सबके लिए खुला है। सभी महात्मा तथा विद्वान् पुरुषों ने गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास द्वारा ही महान् कार्य सम्पादित किये हैं।
(४०) गुरु-भक्ति-योग में अन्य सभी योगों का समावेश है। गुरु-भक्ति-योग का आश्रय लिये बिना कोई भी अन्य योगों — जिन पर चलना कठिन है—का अभ्यास नहीं कर सकता है।
(४१) गुरु-भक्ति-योग की विचारधारा में आचार्योपासना द्वारा गुरु-कृपा प्राप्त करने पर बहुत महत्त्व दिया जाता है।
(४२) गुरु-भक्ति-योग वेद तथा उपनिषद्-काल जितना ही प्राचीन है।
(४३) गुरु-भक्ति-योग जीवन की सभी पीड़ाओं और दुःखों को दूर करने का मार्ग प्रदर्शित करता है।
(४४) गुरु-भक्ति-योग जीवन की व्याधियों की एकमात्र अमोघ औषधि है।
(४५) गुरु-भक्ति-योग का मार्ग मात्र योग्य शिष्य को आशु फलप्रद होता है।
(४६) गुरु-भक्ति-योग की चरम परिणति अहंभाव के नाश तथा अमर आनन्द की उपलब्धि में होती है।
(४७) गुरु-भक्ति-योग सर्वोत्तम योग है।
(४८) गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग प्रणाम करने में संकोच करना गुरु-भक्ति- योग में एक बहुत बड़ी बाधा है।
(४९) आत्म-निर्भरता, आत्मौचित्य, अहम्मन्यता, अभिमान, स्वाग्रह, दीर्घसूत्रता, छिद्रान्वेषण, दुराग्रह, कुसंग, कपट, उद्दण्डता, काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार — ये गुरु-भक्ति-योग में महान् बाधाएँ हैं।
(५०) गुरु-भक्ति-योग के सतत अभ्यास द्वारा मन की अस्थिरता को नष्ट करें।
(५१) गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास द्वारा जब मन की विकीर्ण रश्मियाँ प्रकृतिस्थ हो जाती हैं, तब आप चमत्कारिक कार्य कर सकते हैं।
(५२) गुरु-भक्ति-योग का सिद्धान्त चित्त-शुद्धि प्राप्त करने तथा ध्यान और साक्षात्कार करने के लिए गुरु-सेवा पर अत्यधिक बल देता है।
(५३) सच्चा साधक गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास से आनन्दित होता है।
(५४) प्रथम गुरु भक्ति-योग के तत्त्व-ज्ञान को समझें और तत्पश्चात् उसे चरितार्थ करें, तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी।
(५५) सभी दुर्गुणों के निर्मूलन के लिए एकमात्र प्रभावकारी उपाय गुरु-भक्ति-योग का निष्ठापूर्वक अभ्यास है।
(५६) गुरु में अबाध श्रद्धा गुरु-भक्ति-योग-रूपी वृक्ष का मूल है।
(५७) उत्तरोत्तर वर्धमान भक्ति-भावना, नम्रता, आज्ञाकारिता आदि इस वृक्ष की शाखाएँ हैं, सेवा पुष्प है तथा गुरु को आत्मनिवेदन अगर फल है।
(५८) यदि आपमें सद्गुरु के त्राणदायक चरणों में दृढ श्रद्धा तथा भक्ति-भाव है, तो आपको गुरु भक्ति-योग-साधना में अवश्य सफलता प्राप्त होगी।
(५९) गुरु के प्रति सच्चा तथा हार्दिक समर्पण गुरु-भक्ति-योग का सार है।
(६०) गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास का अर्थ गुरु के प्रति प्रगाढ़ शुद्ध प्रेम है।
(६१) सत्यशीलता के बिना गुरु भक्ति योग में कोई भी प्रगति सम्भव नहीं है।
(६२) गुरु जो कि एक महान् योगी या सिद्ध हो, के उच्चतर आध्यात्मिक स्पन्दनों से युक्त एक शान्त स्थान में निवास करें। तत्पश्चात् उसके तत्त्वावधान में गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास करें। तभी आप गुरु-भक्ति-योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
(६३) गुरु-भक्ति-योग का मूल स्वर ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण-कमलों में अप्रतिबन्ध आत्म-समर्पण है।
(६४) गुरु-भक्ति-योग-दर्शन के अनुसार गुरु तथा भगवान् एक ही है; अतएव गुरु के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण परमावश्यक है।
(६५) गुरु-भक्ति-योग-रूपी निश्रेणी में गुरु के प्रति आत्मसमर्पण निश्चय ही सर्वोच्च सोपान है।
(६६) गुरु-भक्ति-योग में गुरु-सेवा अनिवार्य शर्त है।
(६७) गुरु कृपा गुरु-भक्ति-योग का अन्तिम ध्येय है।
(६८) हठी साधक गुरु-भक्ति-योग की साधना में कोई निश्चित प्रगति नहीं कर सकता है।
(६९) गुरु-भक्ति-योग की साधना करने की इच्छा रखने वाले साधक के लिए कुसंगति एक शत्रु है।
(७०) यदि आप गुरु-भक्ति-योग की साधना करना चाहते हैं, तो विषयी जीवन को त्याग दें।
(७१) जो व्यक्ति दुःख का अतिक्रमण कर जीवन में सुख तथा आनन्द प्राप्त करना चाहता है, उसे गुरु-भक्ति-योग की साधना सच्चाई पूर्वक करनी चाहिए।
(७२) सच्चा स्थायी सुख तो गुरु-सेवा-योग का आश्रय ले कर ही, न कि विनाशशील बाह्य पदार्थों से, प्राप्त किया जा सकता है।
(७३) क्या जन्म तथा मृत्यु के अनवरत चक्र से, सुख-दुःख तथा हर्ष-शोक के द्वन्द्वों से छुटकारा नहीं है? हे शिष्य सुनो! उसका एक अचूक उपाय है। विनाशशील विषय-पदार्थों से अपने मन को पराङ्मुख कर लो और गुरु-सेवा-योग का आश्रय लो। यह तुम्हें द्वन्द्वों से परे ले जायेगा।
(७४) जब मनुष्य गुरु-भक्ति-योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन आरम्भ होता है। जो कोई गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास करता है, उसे इहलोक और परलोक में चिरन्तन सुख प्राप्त होता है।
(७५) गुरु-भक्ति-योग की साधना आपको अपरिमेय तथा अपरिमित आनन्द प्रदान करती है।
(७६) गुरु-भक्ति-योग अपने साधक को चिरायु तथा शाश्वत सुख प्रदान करता है।
(७७) मन संसार अथवा उसकी प्रक्रिया का मूल है। मन ही बन्धन तथा मोक्ष का, सुख तथा दुःख का कारण है। इस मन को गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास द्वारा ही संयम में रखा जा सकता है।
(७८) गुरु-भक्ति-योग अमरत्व, शाश्वत सुख, मुक्ति, पूर्णता, नित्य आनन्द तथा चिरन्तन शान्ति प्रदान करता है।
(७९) परम शान्ति का मार्ग गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास से आरम्भ होता है।
(८०) जो-जो सिद्धियाँ तप, त्याग, योग, दान, पुण्य कर्म आदि से प्राप्त की जा सकती हैं, वे सब गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास से सत्वर ही प्राप्त हो जाती हैं।
(८१) गुरु-भक्ति-योग एक यथार्थ विज्ञान है जो निम्न प्रकृति को वश में करने तथा परम सुख को प्राप्त करने की विधि की शिक्षा देता है।
(८२) कुछ लोग गुरु-सेवा-योग को निम्न कोटि का योग समझते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक रहस्य का पूर्णतया अन्यथा अर्थ ग्रहण किया है।
(८३) गुरु-भक्ति-योग, गुरु-सेवा-योग, गुरु-शरण-योग आदि पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें कोई अर्थ-भेद नहीं है ।
(८४) गुरु-भक्ति-योग सभी योगों का सम्राट् है ।
(८५) गुरु-भक्ति-योग भागवतीय चेतना के लिए सबसे सरल, सुनिश्चित, आशु, सुलभ तथा सुरक्षित मार्ग है। ईश्वर करे, आप सब गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास से इस जन्म में ही भागवतीय चेतना प्राप्त करें!
(८६) गुरु-भक्ति-योग का आश्रय ले कर अपनी खोयी हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करें।
(८७) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास कर द्वन्द्व तथा दुःख-जनक विषयों के परे चले जायें।
(८८) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास शिष्य को परम शान्ति, आनन्द तथा अमरता प्रदान करता है।
(८९) एक वन्य चीते, सिंह अथवा हाथी को पालतू बनाना बहुत सरल है, अनि अथवा जल के ऊपर चलना बहुत सरल है; किन्तु यदि व्यक्ति में गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास की सच्ची आकांक्षा नहीं है, तो उसके लिए सद्गुरु के चरण-कमलों में आत्म-समर्पण करना बहुत कठिन है।
(९०) गुरु-भक्ति-योग मन तथा उसकी वृत्तियों का निरोध है।
(९१) गुरु के प्रति पूर्ण अप्रतिबन्ध आत्म-समर्पण गुरु-भक्ति की प्राप्ति का एक निश्चित मार्ग है।
(९२) गुरु-भक्ति-योग की नींव गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा पर आधारित है।
(९३) यदि आप वास्तव में ईश्वर को चाहते हैं, तो सांसारिक भोगों से पराङ्मुख हो जायें और गुरु-भक्ति-योग के अभ्यास का आश्रय लें।
(९४) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास अनवरत रूप से चालू रखें।
(९५) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास ही मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभय तथा नित्य सुखी बना सकता है।
(९६) गुरु-भक्ति-योग की साधना द्वारा अमर आनन्दमय आत्मा की खोज अपने अन्दर करें।
(९७) गुरु-भक्ति-योग को जीवन का एकमात्र हेतु, उद्देश्य तथा सच्चे रस का विषय बनायें। इससे आप परमानन्द को प्राप्त होगे ।
(९८) गुरु-भक्ति-योग ज्ञान-प्राप्ति में सहायक है।
(९९) गुरु-भक्ति-योग का मुख्य उद्देश्य उच्छृंखल इन्द्रियों तथा भ्रमणशील मन को नियन्त्रित करना है।
(१००) गुरु-भक्ति-योग हिन्दू-संस्कृति की प्राचीन प्रणाली है, जो को शाश्वत सुख के मार्ग पर ले जा कर ईश्वर के साथ आनन्दमय मनुष्य योग कराती है।
(१०१) गुरु-भक्ति-योग आध्यात्मिक तथा मानसिक आत्म-विकास का शास्त्र है।
(१०२) गुरु-भक्ति-योग का उद्देश्य मनुष्य को भौतिकता के चंगुल मुक्त कर उसे दिव्य महिमा तथा अमर आनन्द की मूल स्थिति में पुनः से प्रतिष्ठित करना है।
(१०३) गुरु-भक्ति-योग का अभ्यास शरीर तथा मन को व्याधियों तथा विकारों से मुक्त करता है।
(१०४) गुरु-भक्ति-योग साधक को शारीरिक तथा मानसिक कार्यक्षमता प्रदान करता है।
(१०५) गुरु-भक्ति-योग साधक को दुःख, जरा तथा व्याधि से मुक्त बनाता है तथा उसे चिरायु और शाश्वत सुख प्रदान करता है।
(१०६) गुरु-भक्ति-योग में शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक-सभी प्रकार की साधनाओं का समावेश है, जिनसे व्यक्ति आत्म-संयम तथा आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है।
(१०७) गुरु-भक्ति-योग मन की शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करने का विज्ञान तथा कला है।
(१०८) श्रद्धा तथा भक्ति के पुष्पों से गुरु की पूजा करें।
(१०९) गुरु का सत्संग आत्म-साक्षात्कार के मन्दिर का प्रथम स्तम्भ है।
(११०) ईश्वर-कृपा गुरु का रूप धारण करती है।
(१११) गुरु-दर्शन ही ईश्वर दर्शन है।
(११२) जिसने गुरु का दर्शन नहीं किया है, वह अन्धा ही है।
(११३) धर्म केवल एक ही है और वह है गुरु के प्रति भक्ति तथा प्रेम का धर्म ।
(११४) जब आपमें सांसारिक आशा नहीं रहती, तभी पवित्र आचार्य के प्रति भक्ति-भाव जगता है।
(११५) आध्यात्मिक शिक्षक (गुरु) की संगति से आपका जीवन-संग्राम सरल बन जायेगा ।
(११६) गुरु का आश्रय लें तथा न्यायोचित कार्य करें।
(११७) अपने गुरु की कृपा में श्रद्धा रखें तथा अपने कर्तव्य का पालन करें।
(११८) गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अपनी कब्र खोदना है।
(११९) सद्गुरु शिष्य के लिए सतत वरदान स्वरूप है।
(१२०) जगद्गुरु का हृदय सौन्दर्य का धाम है।
(१२१) जीवन का ध्येय गुरु की सेवा करना है।
(१२२) जीवन का प्रत्येक कटु अनुभव गुरु के प्रति आपके विश्वास की कसौटी है।
(१२३) साधक कार्यों को महत्त्व देता है। गुरु उसके पीछे हेतु तथा उद्देश्य को मापता है ।
(१२४) गुरु के कर्म में शंका करना महापातक है।
(१२५) गुरु के समक्ष अपने दम्भ का प्रदर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए।
(१२६) शिष्य के लिए आज्ञा-पालन जीवन-सिद्धान्त है।
(१२७) अपने दिव्य शिक्षक (गुरु) की सेवा करने का कोई भी अवसर न खोयें।
(१२८) जब आप अपने गुरु की सेवा करें, निष्कपट और गम्भीर रहें।
(१२९) गुरु पर प्रेम रखना गुरु की सेवा करना है।
(१३०) गुरु की सेवा करने के लिए ही जीना चाहिए।
(१३१) गुरु की आज्ञाओं का पालन उनका सम्मान करने से श्रेयस्कर है।
(१३२) आचार्य की आज्ञा का पालन करना त्याग से भी श्रेष्ठ है।
(१३३) प्रत्येक परिस्थिति में अपने गुरु के अनुकूल, समंजित तथा नमनशील बने रहना चाहिए।
(१३४) अपने गुरु के समक्ष अधिक बातचीत न करें।
(१३५) गुरु के प्रति शुद्ध प्रेम गुरु की आज्ञा के पालन का सच्चा स्वरूप है।
(१३६) अपने पास की उत्तमोत्तम वस्तु प्रथम अपने गुरु को अर्पण करें।
(१३७) शिष्य को ईर्ष्या, द्वेष तथा अभिमान से मुक्त, राग-रहित तथा गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति-भाव वाला, अधैर्य-रहित तथा सत्य के साक्षात्कार का निश्चय वाला होना चाहिए।
(१३८) शिष्य को अपने गुरु में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए।
(१३९) शिष्य को अपने गुरु के समक्ष अनावश्यक अथवा निरर्थक बात नहीं करनी चाहिए।
(१४०) आचार्य को यज्ञाति प्रज्वलित करने वाली अरणि के दो काष्ठ- खण्डों में नीचे अथवा मुख्य काष्ठ के रूप में तथा शिष्य को ऊपर के काष्ठ के रूप में समझना चाहिए। उपदेश दोनों को संयुक्त करने वाला मध्य का काष्ठ है तथा ज्ञान सुखजनक योग है।
(१४१) इस प्रकार गुरु से जो सद्ज्ञान प्राप्त होता है, वह माया अथवा भ्रम का निवारण करता है।
(१४२) एक ही ईश्वर माया के कारण अनेक रूप बन गया है, ऐसा ज्ञान जिसे गुरु कृपा से हो गया है, वह सत्य को जानता तथा वेद को समझता है।
(१४३) गुरु की सेवा तथा पूजा द्वारा प्राप्त एकाग्र भक्ति से बने तीक्ष्ण धार वाले ज्ञान- खड्ग से संसार रूपी वृक्ष का शान्तिपूर्वक अविरत गति से उच्छेदन कर डालें।
(१४४) गुरु जीवन-पोत का कर्णधार है और ईश्वर उसे चलाने वाला अनुकूल पवन है।
(१४५) जब मनुष्य में संसार से जुगुप्सा उत्पन्न हो जाती है और उसमें वैराग्य आता है और जब वह अपने गुरु द्वारा प्रदत्त उपदेशों पर चिन्तन करने में समर्थ हो जाता है, तो ध्यान के बारम्बार के अभ्यास के कारण उसका मन अनिष्ट प्रकृति को त्याग देता है।
(१४६) गुरु के पास से उपयुक्त रीति से मन्त्र में दीक्षित होने पर ही मन्त्र-शुद्धि होती है।
(१४७) मनुष्य अनादि काल से अज्ञान के प्रभाव में होने से गुरु के बिना उसे आत्म-साक्षात्कार नहीं हो सकता है। एक ब्रह्मविद् ही दूसरे को ब्रह्मज्ञान प्रदान कर सकता है।
(१४८) बुद्धिमान् मनुष्य को गुरु को आत्मा तथा परमात्मा रूप जान कर असीम भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए।
(१४९) शिष्य में गुरु तथा ईश्वर के प्रति विशुद्ध भक्ति-भाव होना चाहिए।
(१५०) शिष्य को आज्ञाकारिता, सतर्कता तथा निष्कपटता से गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा उनसे भागवत-धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए।
(१५१) शिष्य को गुरु की ईश्वर-रूप में सेवा करनी चाहिए जो कि सर्वेश्वर को प्रसन्न करने तथा उनकी कृपा का अधिकारी बनने का अचूक उपाय है।
(१५२) शिष्य को वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए तथा अपने आध्यात्मिक शिक्षक (गुरु) का सत्संग करना चाहिए।
(१५३) शिष्य को प्रथम अपने गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए और तब उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करना चाहिए।
(१५४) शिष्य को इन्द्रियों को संयम में रख कर गुरु-गृह में निवास करना चाहिए और शास्त्राध्ययन करना चाहिए।
(१५५) शिष्य को गुरु के पवित्र हाथ से जो कोई स्वादिष्ट अथवा सादा, बढ़िया अथवा घटिया, अल्प अथवा पर्याप्त भोजन मिले, उसे खाना चाहिए।
(१५६) मन की निम्न प्रकृति का पूर्ण रूपान्तरण करना चाहिए। साधक अपने गुरु से कहता है : 'मुझे योगाभ्यास करना है। मेरी निर्विकल्प-समाधि में प्रवेश करने की इच्छा है। मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ।' किन्तु वह अपनी निम्न प्रकृति और स्वभाव को, पुराने चरित्र, व्यवहार और आचरण को बदलना नहीं चाहता है।
(१९५७) निम्न प्रकृति का रूपान्तरण सहज नहीं है। आदत की शक्ति सदा बलवती तथा हठीली होती है। इसके लिए बहुत मनोबल की आवश्यकता होती है। प्राचीन स्वभाव की शक्ति से साधक अनेक बार निरुपाय बन जाता है। उसे नियमित जप, कीर्तन, ध्यान, अथक निःस्वार्थ सेवा तथा सत्संग के द्वारा अपने सत्त्व तथा संकल्प का पर्याप्त मात्रा में विकास करना होगा। उसे आत्म-निरीक्षण करके अपने दोषों तथा कमियों का पता लगाना चाहिए। उसे अपने गुरु के मार्ग-दर्शन में रहना चाहिए। गुरु उसके दोषों का पता लगाता है और उनके उन्मूलन का उपयुक्त उपाय निर्देशित करता है।
(१५८) आपको साधन-चतुष्टय से सम्पन्न बन कर ब्रह्मश्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाना चाहिए, उनसे अपनी शंकाओं का निवारण करना चाहिए तथा उनसे प्राप्त आध्यात्मिक प्रकाश की सहायता से आध्यात्मिक मार्ग पर प्रयाण करना चाहिए। जब तक आपका उपयुक्त रूप से गठन न हो जाये, तब तक आपको गुरु के सान्निध्य में ही रहना चाहिए; क्योंकि आत्मसाक्षात्कार प्राप्त आत्माओं का वैयक्तिक सम्पर्क उन्नयनकारी बहुत ही हुआ करता है। यदि आप सच्चे तथा निष्कपट हैं, यदि आपमें ज्वलन्त मुमुक्षुत्व है, यदि आप अपने गुरु के उपदेशों का अति-नियमनिष्ठा से अनुकरण करते हैं, यदि आप सतत तीव्र ध्यान करते हैं, तो निःसन्देह छह माह के भीतर ही आपको परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। आप मेरी बात माह मानें। ऐसा वास्तव में घटित होगा ।
(१५९) यह संसार प्रलोभनों से पूर्ण है; अतएव नव-दीक्षितों को अपनी रक्षा बड़ी सतर्कता से करनी चाहिए। पूर्णतः रूपान्तरित होने तक, गम्भीर ध्यान में प्रतिष्ठित होने तक उन्हें अपने गुरु के चरण-कमलों में बैठना चाहिए। अलमस्त साधक जो प्रारम्भ से ही स्वतन्त्र रहते हैं, जो अपने गुरुओं की वाणी पर ध्यान नहीं देते, वे निराशाजनक नमूने हैं। वे निरुद्देश्य जीवन-यापन करते हैं और सरिता में बह रहे काष्ठ-फलक की भाँति इतस्ततः मारे-मारे फिरते हैं।
(१६०) दुराग्रही साधक अपने प्राक्तन स्वभाव से ही चिपका रहता है। वह ईश्वर अथवा वैयक्तिक गुरु को समर्पण करना नहीं चाहता है।
(१६१) यदि शिष्य वास्तव में अपना सुधार करना चाहता है, तो उसे अपने प्रति सच्चा तथा अपने गुरु के प्रति निष्कपट होना चाहिए।
(१६२) जो अवज्ञाकारी है, जो अनुशासन भंग करता है, जो अपने गुरु से निष्कपट नहीं होता है, जो अपने गुरु के समक्ष अपना हृदय उन्मुक्त नहीं करता है, वह गुरु की सहायता से लाभान्वित नहीं हो सकता है। वह स्व-निर्मित पंक में फँसा रहता है तथा दिव्य पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। क्या ही खेद का विषय है! निश्चय ही उसकी दशा अतीव दयनीय है।
(१६३) शिष्य को ईश्वर अथवा गुरु के प्रति पूर्ण निःशेष मुक्त हृदय से आत्म-समर्पण करना चाहिए।
(२६४) गुरुमात्र यही कर सकता है कि वह अपने शिष्य को सत्य को जानने की विधि अथवा अन्त की शक्ति का उद्घाटन करने वाला मार्ग बतला है।
(१६५) सायन-चतुष्य से सम्पन्न साधक अपने गुरु के चरणों में बैठ कर श्रुतियाँ तथा 'तत्त्वमसि' महावाक्य की अर्थ-व्यंजकता का श्रवण करता है और तब विषय को गम्भीरता से मनन करता है।
(१६५) भगवान् हार, भगवान् शिव, भगवान् कृष्ण, अपने गुरु अथवा भगवान् बुद्ध, प्रभु यीशु जैसे सन्तों में से किसी एक के रूप पर धारणा करें। चित्र की इस मनोमूर्ति को लाने के लिए बारम्बार प्रयास करें। सम्पूर्ण विचार न हो जायेंगे। वह एक अन्य विधि, भक्तों की विधि है।
(१६७) आज्ञाकारिता एक अमूल्य सद्गुण है। यदि आप आज्ञाकारिता के सद्गुण को विकसित करने का प्रयत्न करेंगे, तो आत्म-साक्षात्कार के मार्ग के महाशत्रु, अहं का शनैः-शनैः उन्मूलन हो जायेगा।
(१६८) गुरु की पूर्ण आज्ञाकारिता दुस्साध्य कार्य है, लेकिन सद्भावपूर्वक प्रयास करने से यह बन जाता है।
(१६९) सामान्य कार्य के सम्पादन में भी महान कष्ट होता है। अतएव व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना-पथ में किसी-न-किसी प्रकार के अनुशासन के अधीन रहने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा गुरु की आज्ञाकारिता के पोषण का प्रयास करना चाहिए।
(१७०) आराधना, माल्यार्पण तथा पूजा के द्वारा अपने आन्तरिक भवों की अन्य बाह्य अभिव्यक्तियों की अपेक्षा गुरु की आज्ञाकारिता कहीं महत्तर है।
(१७१) गुरु की आज्ञाकारिता उनके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करती है।
(१७२) आज्ञाकारिता का अर्थ है—गुरु जिस प्रकार कार्य करने की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार कार्य करने का प्रयास करना।
(१७३) यदि किसी को यह पता चल जाये कि गुरु अमुक कार्य पसन्द नहीं करते, तो व्यक्ति को उस कार्य को नहीं करना चाहिए। यह भी आज्ञाकारिता है।
(१७४) गुरु-सेवा गुरु के प्रति किया गया निष्काम सेवा-योग है।
(१७५) गुरु की सेवा मानवता की सेवा है।
(१७६) गुरु-सेवा मन की मलिनता का निवारण करती है। यह प्रभावकारी अन्तःकरण-शुद्धिकारक है। अतः गुरु की भाव तथा बोधपूर्वक सेवा कीजिए।
(१७७) गुरु-सेवा मन को दिव्य ज्योति, ज्ञान तथा कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है।
(१७८) गुरु-सेवा हृदय को विकसित करती तथा सभी अपराधों को ध्वस्त करती है। यह चित्त-शुद्धि के लिए प्रभावकारी साधना है।
(१७९) गुरु-सेवा मन को सदा गतिशील तथा सतर्क रखती है।
(१८०) गुरु-सेवा करुणा, विनम्रता, आज्ञाकारिता, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, आत्म-त्याग आदि दिव्य सद्गुणों के विकास में व्यक्ति की सहायता करती है।
(१८१) गुरु-सेवा ईर्ष्या, घृणा तथा श्रेष्ठता - मनोग्रन्थि को नष्ट करती है।
(१८२) अपने गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति 'अहन्ता' तथा 'ममता' पर विजय पा लेता है।
(१४३) जो शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, वह वस्तुतः अपनी सेवा करता है।
(१८४) गुरु-सेवा-योग की साधना में अनिर्वचनीय सुख तथा शान्ति है।
(१८५) गुरु-सेवा के लिए जियें ।
(९८६) प्रातः चार बजे उठ जायें। यह गुरु की मूर्ति पर ध्यान करने का अनुकूल समय है।
(१८७) शिष्य को अपने गुरु-गृह में निवास करते समय सन्तुष्ट जीवन-यापन करना चाहिए। उसमें पूर्ण आत्म-संयम होना चाहिए।
(१८८) शिष्य को गुरु के समक्ष मृदु, मधुर तथा सत्य बोलना चाहिए और अशिष्ट तथा परुष वचन नहीं बोलना चाहिए।
(१८९) शिष्य को अपने गुरु की पीठ पीछे निन्दा नहीं करनी चाहिए।
(१९०) जो अपने गुरु की पीठ पीछे निन्दा करता है, वह रौरव नरक में जाता है।
(१९१) जो व्यक्ति भोजन के लिए जीता है, वह पापी है; किन्तु जो व्यक्ति अपने गुरु की सेवा के लिए भोजन करता है, वह सच्चा शिष्य है।
(१९२) जो गुरु का ध्यान करता है, उसे मिताहार की आवश्यकता होती है।
(१९३) गुरु-सेवा के अभाव में सच्छास्त्रों का अध्ययन केवल समय
(१९४) गुरु दक्षिणा दिये बिना गुरु से शास्त्रों का अध्ययन करना समय नष्ट करना है।
(१९५) गुरु की इच्छाओं की पूर्ति किये बिना वेदान्त-पाठ उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्रों का मात्र अध्ययन न तो कल्याणकारी होगा और न बोधप्रद ही।
(१९६) चिर काल तक सेवा करने से शुद्ध तथा शान्त पर व्यक्ति का गुरु बन जाता है।
(१९७) भले ही आप जितना चाहें उतने ही दार्शनिक ग्रन्थों का परिशीलन करें, अपनी विश्वयात्रा- भर प्रवचन करें, हिमालय की कन्दराओं ये सहस्रों वर्ष तक निवास करें, वर्षों तक प्राणायाम की साधना करें, आजीवन शीर्षासन करें; पर गुरु कृपा के बिना आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
(१९८) यद्यपि गुरु के लिए ब्रह्म को 'इदं' कह कर इंगित कर पाना तथा शिष्य के लिए अपरोक्षानुभूति से पूर्व ब्रह्म के स्वरूप का बोध कर पाना सम्भव नहीं है; किन्तु गुरु-कृपा शिष्य को रहस्यमय ढंग से अपने अन्दर ब्रह्म-तत्त्व की अपरोक्षानुभूति के लिए समर्थ बना देती है।
(१९९) आपके गुरु ही आपके माता, पिता और गुरु जन हो।
(२००) यदि गुरु अनुमति दें, तो उनके चरणों की मालिश करें।
(२०१) प्रत्येक व्यक्ति को गुरु तथा वेदान्त-वाक्यों के यथार्थ अर्थ के बोध की सहायता से अपने ही ज्ञान द्वारा अपने अन्दर आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए।
(२०२) व्यक्ति के गुरु हों, तब भी उसे अपने ही प्रयत्नों द्वारा सम्पूर्ण कामनाओं, वासनाओं तथा अहंकार को नष्ट करना तथा आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए।
(२०३) गुरु के पास जाने के लिए आपको उपयुक्त अधिकारी होना चाहिए। आपको वैराग्य, शम, दम तथा यम से सम्पन्न होना चाहिए।
(२०४) यदि आप कहते हैं, 'सद्गुरु नहीं हैं', तो गुरु भी कहते हैं, 'सद्शिष्य नहीं हैं।' शिष्य के गुणों से सम्पन्न बनिए। आपको सद्गुरु प्राप्त होंगे।
(२०५) गुरु आपके उद्धारक तथा परित्राता हैं। सदा उनकी आराधना तथा पूजा करें।
(२०६) गुरुपन एक भयंकर अभिशाप है।
(२०७) अपने गुरु के समक्ष प्रतिदिन साष्टांग प्रणाम करें। वह परम सत्, चित् तथा आनन्द हैं।
(२०८) शिष्य को सदा गुरु की मूर्ति का ध्यान, गुरु के पवित्र नाम का जप तथा उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। उनके अतिरिक्त अन्य किसी का चिन्तन नहीं करना चाहिए। यही साधना के रहस्य के मूल में है।
(२०९) व्यक्ति को अपने गुरु की आराधना करनी चाहिए; क्योंकि उनसे महत्तर कुछ भी नहीं है।
(२१०) गुरु का चरणामृत संसार-सागर का शोषण कर लेता है तथा व्यक्ति को आत्मा की महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।
(२११) गुरु का चरणामृत शिष्य की पिपासा को शमित करता है।
(२१२) जब आप ध्यान के लिए बैठे तो अपने सभी सम के सन्तों को स्मरण करें। आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा।
(२१३) महात्माओं की विवेकपूर्ण वाणी को सुनिए तथा उसका पालन कीजिए।
(२१४) शास्त्र तथा गुरु विहित सत्कर्म ही कीजिए।
(२१५) शान्ति का पथ प्रदर्शित करने के लिए गुरु की नितान्त आवश्यकता है।
(२१६) 'वाहे गुरु' गुरु नानक के अनुयायियों का गुन है। ग्रन्थसाहिब का अध्ययन करें। आपको गुरु की महता ज्ञात हो जायेगी।
(२१७) गुरु की पूजा द्वारा उन्हें सदा स्मरण रखें। आपको सुख प्राप्त होगा।
(२१८) शास्त्रों, गुरु की वाणी, ईश्वर तथा स्वयं में आस्तिक-बुद्धि श्रद्धा है।
(२१९) सर्वोत्कृष्ट साधना निष्काम भाव से गुरु की सेवा करना है।
(२२०) श्रवण का अर्थ है सद्गुरु के चरण-कमलों में बैठकर श्रुतियों को सुनना ।
(२२१) गुरु की सेवा महान् शुद्धिकारिणी है।
(२२२) आत्म-साक्षात्कार के लिए गुरु कृपा आवश्यक है।
(२२३) जितनी भक्ति-भावना आप प्रभु के प्रति रखते हैं, उतनी ही गुरु के प्रति भी रखें। तभी सत्य आपके हृदय में प्रकाशित होगा।
(२२४) सदा एक ही गुरु के पास टिके रहें।
(२२५) ईश्वर आद्य गुरु हैं, जिन्हें दिक्काल का बन्धन नहीं है। वह अनादि काल से शाश्वत काल तक मानव-जाति के गुरु है।
(२२६) कुण्डलिनी शक्ति को उसकी सुषुप्तावस्था से जाग्रत करने के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता होती है।
(२२७) शिष्यत्व का आरम्भ अहन्ता का विनाश है।
(२२८) शिष्यत्व की कुंजी ब्रह्मचर्य तथा गुरु-सेवा है।
(२२९) शिष्यत्व का परिधान गुरु-भक्ति है।
(२३०) शिष्यत्व का चिह्न गुरु के चरण-कमलों में जीवन समर्पण है।
(२३१) शिष्यत्व का राजपथ गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान है।
(२३२) शिष्यत्व का आधार गुरु महाराज की पूर्ण आज्ञाकारिता है।
(२३३) गुरु को मिलने तथा उनकी सेवा करने की ज्वलन्त कामना मुमुक्षुत्व है।
(२३४) देवों, द्विजों, गुरुओं तथा ज्ञानियों की पूजा, शुचिता, ऋजुता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शरीर के तप हैं।
(२३५) ब्राह्मणों, पवित्र गुरुओं तथा ज्ञानी पुरुषों को प्रणाम करना, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शारीरिक तप हैं।
(२३६) माता, पिता, गुरुओं, निर्धनों तथा रोगियों की सेवा भी शरीर की तपश्चर्याएँ हैं।
(२३७) अनुकूल होने का गुण बहुत ही विरल होता है और यह एक श्रेष्ठ गुण है। इससे शिष्य, भले ही उसका स्वभाव कैसा भी क्यों न हो, अपने को गुरु के अनुकूल बना लेता है।
(२३८) आजकल अधिकांश साधकों को अपने को अपने गुरुभाइयों के अनुकूल बनाने अथवा उनके साथ समन्वय करने का ज्ञान नहीं है।
(२३९) शिष्य को अपने गुरु के अनुकूल बनना तथा उनके साथ हिल-मिल जाना चाहिए।
(२४०) गुरु-भक्ति-योग के विकास के लिए विनम्रता तथा आज्ञाकारिता आवश्यक है।
(२४१) जब शिष्य एक गुरु के अधीन रहने वाले सहशिष्यों के अनुकूल बनना नहीं जानता, तो संघर्ष उत्पन्न होता है और अपने गुरु को अप्रसन्न कर देता है।
(२४२) जलपोत का अधिपति सदा सतर्क रहता है। धीवर सदा सतर्क रहता है। शल्यचिकित्सक शल्यशाला में सदा सतर्क रहता है। इसी भाँति पिपासु तथा क्षुधित शिष्य को अपने गुरु की सेवा में सदा सतर्क रहना चाहिए।
(२४३) निद्रालु, निरुत्साह, उदास, अकर्मण्य, सुस्त तथा जड़मति शिष्य अपने गुरु की सन्तोषप्रद रूप से सेवा नहीं कर सकता है।
(२४४) अध्यवसाय गुण से सम्पन्न शिष्य अपने गुरु की सेवा में सफल होता है। समृद्धि तथा अमरता उसके परिचर हैं।
(२४५) शिष्य में अपने गुरु की सेवा करने की आकांक्षा अथवा ज्वलन्त कामना होनी चाहिए।
(२४६) गुरु के प्रति भक्ति मानव की सभी शुभ महत्त्वाकांक्षाओं का एकमात्र वास्तविक ध्येय है।
(२४७) जब शिष्य गुरु के पास अध्ययन करता हो, तो उसके श्रोत्र सावधान होने चाहिए और जब वह गुरु की सेवा करता हो, तो उसकी दृष्टि सावधान होनी चाहिए।
(२४८) शिष्य को अपने गुरु, माता-पिता, गुरु जनों तथा सभी काल के सन्तों और ज्ञानी जनों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए।
(२४९) सद्व्यवहार का अर्थ है गुरु के साथ सदाचरण ।
(२५०) गुरु शिष्य के व्यवहार से उसके स्वभाव तथा उसके मन के स्वरूप को जान सकता है।
(२५१) अपने पावन गुरु के प्रति सद्व्यवहार आनन्दधाम का पारपत्र है।
(२५२) गुरु की सेवा करते समय शिष्य को मनमौजी नहीं होना चाहिए।
(२५३) आचार अपने गुरु की सेवा से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान की अभिव्यक्ति है।
(२५४) दैवी सम्पद् तथा सद्गुण दुकानों से क्रय नहीं किये जा सकते हैं। ये तो दीर्घ काल तक गुरु-सेवा, श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं।
(२५५) आप महान् विद्वान् तथा धनाढ्य हों, तो भी गुरु तथा महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही विनीत होना चाहिए।
(२५६) शिष्य बहुत विद्वान् न हो, पर यदि वह विनम्रता का साकार रूप हो, तो उसके गुरु का उसके ऊपर अत्यधिक स्नेह होता है।
(२५७) यदि आप नल से जल पीना चाहते हैं, तो आपको नीचे झुकना होगा। इसी भाँति यदि आप गुरु के पवित्र मुख से प्रवाहित अमरत्व की अध्यात्म-सुधा का पान करना चाहते हैं, तो आपको विनम्रता तथा विनयशीलता की मूर्ति बनना होगा।
(२५८) जो मनुष्य विनम्र तथा निष्ठावान् होते हैं, उनके ऊपर ही गुरु की कृपा का अवतरण होता है।
(२५९) गुरु के चरण-कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प श्रेष्ठतर अन्य कोई पुष्प नहीं है।
(२६०) श्रद्धा गुरु में विश्वास तथा निष्ठा को कहते हैं।
(२६१) श्रद्धा अपने पवित्र गुरु तथा महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखों तथा उपदेशों में विश्वास है।
(२६२) गुरु साक्षी अथवा अधिकारी व्यक्ति के रूप में जो कहे, उसमें किसी साक्ष्य अथवा प्रमाण की चिन्ता किये बिना दृढ़ विश्वास रखना श्रद्धा है।
(२६३) गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखें और अपनी सम्पूर्ण सत्ता को उन्हें समर्पित कर दें। वह आपकी सँभाल करेंगे। उससे सम्पूर्ण भय, अन्तराय तथा कष्ट पूर्णतया नष्ट हो जायेंगे।
(२६४) सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा आत्मा को उन्नत करती, हृदय को शुद्ध बनाती तथा जीव को आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाती है।
(२६५) गुरु के उपदेशों में भाव-प्रवण श्रद्धा शिष्य का आदर्श वाक्य होना चाहिए। -
(२६६) आज्ञाकारिता गुरु तथा गुरु जनों के आदेशों के पालन की तत्परता है।
(२६७) जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वहीं अपनी निम्न आत्मा पर शासन कर सकता है।
(२६८) नम्रता, भक्ति-भाव, निरहंकारिता आदि अन्य सभी गुण गुरु की आज्ञा के पालन से उत्पन्न होते हैं।
(२६९) गुरु के आदेशों में शंका न करना तथा उनके पालन में विलम्ब न करना गुरु की सच्ची आज्ञाकारिता है।
(२७०) गुरु की आज्ञाओं का पालन सभी अध्यवसायों में सफलता की जननी है।
(२७१) गुरु जिसकी आज्ञा दें, उस कार्य को करना तथा जिसे निषेध करें, उस कार्य को न करना ही गुरु की सच्ची आज्ञाकारिता है।
(२७२) दम्भी शिष्य भयवश अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, सच्चा शिष्य प्रेम के लिए, शुद्ध प्रेम से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है।
(२७३) शिष्य का प्रथम पाठ गुरु की सच्ची आज्ञाकारिता है।
(२७४) भलाई एक सरिता है जो की आज्ञा-पालन के मार्ग से ईश्वर के चरण-कमलों से प्रवाहित होती है।
(२७५) यदि शिष्य के हृदय में सन्तोष न हो, तो यह प्रकट करता है कि शिष्य ने गुरु की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है।
(२७६) आपमें भाव तथा उत्साह होगा, तो गुरु आपकी भेंट से प्रसन्न होंगे, न कि आपकी भेंट के प्रकार से।
(२७७) शिष्य को अपने गुरु की सेवा बहुत उत्साह तथा मनोयोगपूर्वक करनी चाहिए।
(२७८) यदि साधक श्रद्धा तथा भक्ति-भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करता, तो उसके सभी व्रत तथा तप उसी भाँति क्षीण हो जायेंगे जैसे कच्चे घड़े में रखा हुआ जल टपक जाता है।
(२७९) मन तथा इन्द्रियों का सयम, गुरु-भगवान् का ध्यान करना, गुरु की सेवा करने में धैर्य, सहनशीलता, गुरु के प्रति भक्ति-भाव, सन्तोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, ऋजुता तथा गुरु की आज्ञाकारिता-ये सब सच्छिष्य के लक्षण हैं।
(२८०) सत्य के जिज्ञासु को मन तथा इन्द्रियों के ऊपर संयम रख कर अपने आचार्य के घर में रहना चाहिए तथा आदरपूर्वक उनके अधीन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए।
(२८१) उसे कठोर ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना चाहिए तथा गुरु पूजा करनी चाहिए। की
(२८२) शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को मनुष्य-रूप में न देख कर उन्हें साक्षात् भगवान् माने ।
(२८३) शिष्य को गुरु के दोष नहीं देखने चाहिए; क्योंकि गुरु सभी देवों का प्रतिनिधि है।
(२८४) शिष्य को गुरु के लिए भिक्षा माँग कर लानी चाहिए और उन्हें बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से खिलाना चाहिए।
(२८५) शिष्य को सभी सुख-सुविधाओं को त्याग देना चाहिए और अपने शरीर को गुरु की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए।
(२८६) शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात् शिष्य को अपने को दक्षिणा देनी चाहिए और उनकी अनुमति से अपने घर वापस जाना चाहिए।
(२८७) जो गुरु-पद का उपयोग आजीविका के साधन के रूप में करता है, वह धर्म का नाश करने वाला है।
(२८८) ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य अपने आचार्य की पूर्ण हृदय से निःस्वार्थ सेवा करना है।
(२८९) गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी व्यक्तिगत सेवा तथा उनकी पूर्ण आज्ञाकारिता जितनी सहायप्रद है, उतना सहायप्रद तप, तीर्थयात्रा, भेंट, दान नहीं है।
(२९०) वेद, अपरोक्ष ज्ञान, गुरु-वचन तथा अनुमान —ये ज्ञान के चार प्रमाण हैं।
(२९१) प्रत्येक कर्म में दुःख के बीज निहित हैं, किन्तु गुरु की सेवा के विषय में यह बात नहीं है।
(२९२) गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए शिष्य को किसी समय भी धन, भोग-विलास, सुख-सुविधा तथा अपने शरीर तक का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
(२९३) जो तन, मन तथा धन गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, वह गुरु भक्ति योग विकसित करता है।
(२९४) जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति-भाव की वृद्धि हो, वह परम धर्म है।
(२९५) गुरु-मन्त्र का जप, गुरु-सेवा-काल में तपश्चर्या, गुरु-वचन में श्रद्धा, आचार्य-सेवन, सन्तोष, शुचिता, शास्त्र-परिशीलन तथा गुरु-भक्ति अथवा गुरु को आत्म-समर्पण - ये नियम हैं।
(२९६) गुरु के आदेशों के पालन करने में कष्ट सहन करना तितिक्षा है।
(२९७) गुरु ने जिस कर्म का निषेध किया हो, उस कर्म को छोड़ देना त्याग है।
(२९८) गुरु की व्यक्तिगत सेवा करने से शिष्य अपने मन को वश में कर सकता है।
(२९९) गुरु के भोजन कर लेने के पश्चात् जो आहार बचा रहता है, वह सर्वाधिक सात्त्विक भोजन है।
(३००) गुरु इस भूलोक में साक्षात् ईश्वर हैं तथा वह सच्चे मित्र तथा विश्वासपात्र सम्बन्धी हैं।
परिशिष्ट
गुरु-गीता का सार
मंगलाचरणं शिष्टाचाराद्वै फलदर्शनात् ।
शिष्ट लोगों का आचार है कि फल की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए।
मंगलं भगवान् विष्णुमंगलं गरुडध्वजः ।
मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनं हरिः ।। १ ।।
भगवान् विष्णु मंगल करने वाले हैं। भगवान् जो गरुड़ पर सुशोभित हैं मंगल करने वाले हैं। भगवान् जो कमल-नयन हैं मंगलकारक हैं। भगवान् हरि मंगल को बढ़ाने वाले हैं।
सच्चिदानन्दकन्दाय जगदंकुरहेतवे ।
सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनन्ताय विष्णवे ॥ २ ॥
अनन्त विष्णु को प्रणाम है जो सदैव उदित एवं पूर्ण हैं, जो समस्त जगत् के अंकुर - कारण हैं, जो सत्-चित्-आनन्द के महत्तम द्योतक हैं।
सत्यानन्दस्वरूपाय बोधैकसुखकारिणे ।
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥ ३ ॥
गुरु को साष्टांग प्रणाम है जो बुद्धि का साक्षी है, जो वेदान्त द्वारा ज्ञेय है, जो चेतनानन्द का साधन है, जो सत्यानन्द का स्वरूप है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ||४||
गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु है। गुरु भगवान् महेश है। गुरु प्रत्यक्ष रूप परम ब्रह्म है। उस गुरु को प्रणाम है।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥५ ॥
अन्धे की आँखों को ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अन्धकार अंजनशलाका से खोलने वाले उस गुरु को साष्टांग प्रणाम है।
स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित्सचराचरम् ।
त्वंपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ||६||
जो चल और अचल सृष्टि में स्थिर एवं अस्थिर जीवों में व्याप्त है, जिसने 'तू' शब्द का दर्शन कराया है, उस गुरु को प्रणाम है।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥७ ॥
जो स्थिर और अस्थिर सृष्टि में अखण्डमण्डलाकार रूप में व्याप्त है। जिसने 'वह' शब्द का दर्शन कराया है, उस गुरु को प्रणाम है।
चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ।
असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥८ ॥
जो चिन्मय स्वरूप तीनों लोकों के चल एवं अचल सब निवासियों में व्याप्त है, जिसने 'तू है' का दर्शन कराया है, उस गुरु को प्रणाम है।
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरंजनम् ।
नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥९॥
जो चैतन्य, शाश्वत, शान्त, व्योम से परे है, निरंजन है, जो नाद, बिन्दु और कला से परे है, उस गुरु को प्रणाम है।
यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति यत् ।
यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ।। १० ।।
जिसके अस्तित्व से संसार का अस्तित्व है, जिसके प्रकाश से जगत् प्रकाशित होता है, जिसके आनन्द से सब आनन्दित हैं, उस गुरु को प्रणाम है।
न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः ।
न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरवे नमः ।। ११ ।।
गुरु से बढ़ कर कोई तत्त्व नहीं, गुरु से बढ़ कर कोई तप नहीं, गुरु से बढ़ कर कोई ज्ञान नहीं, उस गुरु को प्रणाम है।
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ।। १२ ।।
ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है, पूजा का मूल गुरु के चरण हैं। मन्त्रों का मूल गुरु-वाक्य है और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है।
गुरुपादोदकं पानं गुरोरुच्छिष्टभोजनम् ।
गुरुमूर्तेः सदा ध्यानं गुरोर्नाम सदा जपः ॥१३॥
गुरु के चरण-प्रक्षालित जल का पान करना चाहिए। गुरु के भोजन के बाद बचा हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। गुरु की मूर्ति का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। गुरु के नाम का प्रतिदिन जप करना चाहिए।
अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणम् ।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरोः पादोदकं पिबेत् । । १४॥
ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति हेतु गुरु-चरण-प्रक्षालित जल का पान करना चाहिए, जो अज्ञान के मूल को दूर करता है, जो जन्म एवं कर्मों के धनों का निवारण करता है।
काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम् ।
गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयम् ।। १५ ।।
काशी क्षेत्र निवास स्थल है, गंगा जल उसके चरणों के लिए जल है, साक्षात् महेश्वर गुरु है। तारक-मन्त्र निश्चित रूप से परम ग्रहा है।
आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकम्।
साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारणम् ।। १६ ।।
साधक को गुरु के सन्तोष हेतु गुरु को आसन, शयन-सामग्री, वस्त्र, बाहन, आभूषण आदि भेंट करने चाहिए।
शरीरमिन्द्रियं प्राणानर्थस्वजनबान्धवान् ।
आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् ।।१७।।
अपना शरीर, इन्द्रियाँ, जीवन, सम्पत्ति, मित्र, सम्बन्धी, आत्मा, पत्नी - सब कुछ गुरु चरणों में निवेदित कर देना चाहिए।
गुरुरेको जगत्सर्व ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम् ।
गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेद् गुरुम् ।। १८ ।।
ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित एक गुरु सारा संसार है। गुरु से महान् कोई नहीं है, अतः गुरु की पूजा करनी चाहिए।
कर्मणा मनसा वाचा सर्वदाऽऽराधयेद् गुरुम् ।
दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ ।। १९ ।।
गुरु के समक्ष बिना संकोच के लम्बा दण्डवत् प्रणाम करना चाहिए और मन,कर्म तथा वचन से हमेशा आराधना करनी चाहिए।
सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं यथा ।
गुरुपादपयोबिन्दोश्च सहस्रांशेन तत्फलम् ।। २० ।।
सात समुद्रों तक के तीर्थ-स्नानों का फल गुरु-चरणों के प्रक्षालन से प्राप्त एक बूँद पान के हजारवें अंश के समान है।
शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरी रुष्टे न कश्चन ।
लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यग् गुरुमेव समाश्रयेत् ।। २१ ।।
भगवान् के नाराज होने पर गुरु रक्षक है, गुरु के नाराज होने पर कोई रक्षक नहीं है। अतः कुल-गुरु प्राप्त करके उस उपयुक्त गुरु का ही आश्रय ले लेना चाहिए।
श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते ।
तस्यां दिशि नमस्कुर्याद् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये ।। २२ ।।
जिस दिशा में लक्ष्मी-पति के चरणयुगल सुशोभित होते हैं, हे प्यारे! उस दिशा में प्रतिदिन भक्तिपूर्वक प्रणाम करना चाहिए।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ २३ ॥
उस सद्गुरु को साष्टांग प्रणाम करता हूँ जिसकी सत्ता तीन गुणों से रहित है, जो भाव से परे है, सम्पूर्ण मानसों में व्याप्त, परिवर्तन-रहित, निर्मल, एक और नित्य, द्वन्द्व से परे, गगनसदृश विशाल, 'तू वह है' जैसे आदि-वाक्यों से सुलभ, ब्रह्मानन्द, परम सुख का दाता, ज्ञान की मूर्ति है।
आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं
ज्ञानस्वरूपं निजभाव युक्तम् ।
योगीन्द्र मीड्यं भवरोग वैद्यं
श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि ।। २४ ।।
मैं हमेशा प्रभु-प्रिय गुरु को प्रणाम करता हूँ जो संसार रूपी रोग के वैद्य हैं, जो योगियों के आराध्य देव हैं, जो आनन्दमय हैं, जो सदैव प्रसन्न हैं, जो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, जो यथार्थ सत्ता से एकात्म हैं।
हृदम्बुजेकर्णिकमध्यसंस्थ
सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिम् ।
ध्यायेद् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं
सच्चित्सुखाभीष्टवरं दधानम् ।। २५ ।।
दिव्य रूप गुरु का ध्यान करना चाहिए, जो हृदय-रूपी कमल के मध्य में सुशोभित हैं, जो भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं, जो चन्द्रकला की अभीष्ट वरदान को देने के भाँति प्रकाशवान् हैं, जो सत्-चित्-आनन्द लिए तत्पर हैं ।
नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम् ।
नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम् || २६ ।।
मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ, जो ब्रह्म है, चिदानन्द है, नित्य ज्ञानवान् है, दोष-रहित है, निराकार है, निरंजन (दृष्टि से परे) है, नित्य-निर्मल तथा अदृश्य है ।
गुरुं त्वंकृत्य हुंकृत्य गुरुसान्निध्यभाषणः ।
अरण्ये निर्जले देशे सम्भवेद् ब्रह्मराक्षसः || २७ ।।
वह जो गुरु को 'तू' कह कर और अपने को 'हम' कह कर सम्बोधित करता है, गुरु की उपस्थिति में अधिक बोलता है, वह जल-हीन अरण्य-क्षेत्र में ब्रह्मराक्षस (एक भयंकर राक्षस) बनता है।
नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत्परम् ।
भासयन् ब्रह्मभावं च दीपो दीपान्तरं यथा ।। २८ ।।
दीपक का दीपक से अन्तर जैसे ही ब्रह्म-भाव को प्रकट करते हुए उस नित्य, निराकार, निर्गुण परम ब्रह्म को जानना चाहिए।
वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भावातीतं जगद्गुरुम् ।
नित्यं पूर्ण निराकारं निर्गुणं त्वात्मसंस्थितम् ।। २९ ।।
मैं सच्चिदानन्द की वन्दना करता हूँ जो भाव से परे है, जगत् का गुरु है, नित्य, पूर्ण, निराकार, निर्गुण, किन्तु आत्माओं में स्थित है।
गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणाम् ।
गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्न विद्यते ।। ३० ।।
गुरु शिव है। गुरु ईश्वर है। गुरु शरीरधारियों का बन्धु (मित्र) है। गुरु आत्मा है। गुरु जीव है। गुरु के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः ।
स्वविश्रान्तिं न जानाति परशान्तिं करोति किम् ।। ३१ ।।
ज्ञान-हीन, मिथ्यावादी और पाखण्डी गुरु त्याज्य है । वह स्वयं यह नहीं जानता कि शान्ति क्या है तो दूसरों को किस प्रकार शान्ति प्रदान कर सकता है।
पाखण्डिनः पापरता नास्तिका भेदबुद्धयः ।
स्त्रीलम्पटा दुराचाराः कृतघ्ना बकवृत्तयः ॥ ३२ ॥
वे गुरु नहीं हैं जो पाखण्डी हैं, जो पाप में रत रहते हैं, नास्तिक हैं,भेद-भाव स्वरूप हैं, जो स्त्री-लम्पट हैं, जो दुराचारी हैं, कृतघ्न और कपटी हैं।
निरस्तसर्वसन्देहमेकीकृत्य सुदर्शनम् ।
रहस्यं यो दर्शयति भजामि गुरुमीश्वरम् ।। ३३ ।।
मैं गुरु-रूप ईश्वर का भजन करता हूँ, जो समस्त दर्शनीय विषयों को एक कर, शंकाओं का समाधान कर रहस्य का दर्शन कराता है।
गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः ।
तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यहृत्तापहारकम् ।। ३४ ।।
अपने शिष्यों से धन खींचने वाले बहुत से गुरु हैं; किन्तु शिष्य के हृदय का दुःख दूर करने वाले उस एक को दुर्लभ मानता हूँ।
चातुर्यवान् विवेकी च अध्यात्मज्ञानवांछुचिः ।
मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते ||३५||
उसका गुरुत्व वास्तविक शोभित होता है जिसका निर्मल मस्तिष्क चातुर्यवान्, विवेकशील, अध्यात्म-ज्ञान से पूर्ण और पवित्र है।
गुरवो निर्मलाः शान्ताः साधवो मितभाषिणः ।
कामक्रोधविनिर्मुक्ताः सदाचाराः जितेन्द्रियाः || ३६ ।।
गुरु जन निर्मल, शान्तिमय, सज्जन, मितभाषी, काम-क्रोध से मुक्त,सदाचारी एवं जितेन्द्रिय होते हैं।
एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नैव मन्यते ।
शुनां योनिशतं गत्वा चण्डालेष्वभिजायते ।। ३७ ।।
एक अक्षर (ॐ) को देने वाले गुरु को जो नहीं मानता है, वह सैकड़ों जन्मों तक कुत्ते की योनि में जा कर चाण्डालों के वंश में जन्म लेता है।
गुरुत्यागाद्भवेन्मृत्युर्मन्त्रत्यागाद्दरिद्रता ।
गुरुमन्त्रपरित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत् ।। ३८ ।।
गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मन्त्र के त्याग से निर्धनता सताती है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मन्त्र को छोड़ने वाला रौरव नरक में जाता है।
सप्तकोटिमहामन्त्राश्चित्तविभ्रमकारकाः ।
एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम् ।। ३९ ।।
सात करोड़ महामन्त्र मन को भ्रमित करने वाले हैं। दो अक्षरों का 'गुरु' ही एकमात्र महामन्त्र है।
गुकारश्चान्धकारश्च रुकारस्तन्निरोधकृत् ।
अन्धकारविनाशित्वाद् गुरुरित्यभिधीयते ।। ४० ।।
'गु' अक्षर अन्धकार है, 'रु' अक्षर उसका निवारक है। अन्धकार का विनाश करने से ही 'गुरु' यह संज्ञा रखी जाती है।
श्रद्धालुर्मुक्तिवाक्येषु वेदान्तज्ञानलिप्सया ।
उपायनकरो भूत्वा गुरुं ब्रह्मविदं व्रजेत् ।। ४१ ।।
मुक्ति-वाक्यों में श्रद्धा रखने वाला वेदान्त - ज्ञान की इच्छा से उपहार ले कर ब्रह्म को जानने वाले गुरु की शरण में जाये।
श्रवणं तु गुरोः पूर्व मननं तदनन्तरम् ।
निदिध्यासनमित्येतत् पूर्णबोधस्य कारणम् ।। ४२ ॥
प्रथम गुरु के समक्ष श्रवण करना चाहिए। तदनन्तर उस पर (यह क्या शब्द है) मनन करना चाहिए। तब पूर्ण चिन्तन पूर्ण ज्ञान का कारण बनता है।
यथा यथा जात्यन्धस्य रूपज्ञानं न विद्यते ।
तथा गुरूपदेशेन विना ज्ञानं न विद्यते ॥ ४३ ॥
जिस प्रकार जन्म से अन्धे मनुष्य को रूप का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार गुरु के उपदेश के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं होता है।
यदा सद्गुरुकटाक्षो भवति
तदा भगवत्कथाश्रवणध्यानादौ श्रद्धा जायते ।
शान्तो दान्तोऽतिविरक्तः
सुश्रद्धो गुरुभक्तस्तपोनिष्ठः || ४४ ॥
जब गुरु की कृपा होती है, तब भगवत् कथाओं के श्रवण, ध्यान आदि में श्रद्धा का उदय होता है। साधक को क्षोभ रहित, जितेन्द्रिय, पूर्ण विरक्त, श्रद्धायुक्त, गुरु भक्त और तप में स्थिर होना चाहिए।
शिष्यो ब्रह्मनिष्ठं गुरुमासाद्य प्रदक्षिणपूर्वकं
दण्डवत् प्रणम्य प्रांजलिर्भूत्वा विनयेनोपसंगम्य ।
भगवन् गुरो मे परमतत्त्वरहस्यं
विविधं वक्तव्यमिति ।। ४५ ।।
साधक को ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में पहुँच कर उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हुए, साष्टांग दण्डवत् तथा करबद्ध प्रणाम कर, अति-विनयी हो कर निवेदन करना चाहिए, “हे प्रभो, हे गुरु, मुझे परम तत्त्व का पूर्ण रहस्य विस्तार से बतलाने की कृपा करें।"
सर्वज्ञं सर्वगं शान्तं सर्वेषां हृदये स्थितम् ।
संवेद्यं गुरुमुखात् सुदुर्बोधमचेतसाम् ||४६ ॥
दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरम् ।
पूजयेत्परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत् ।। ४७ ।।
जो परम श्रद्धा से उस गुरु की पूजा करता है, जो सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र व्याप्त, शान्त, सबके हृदय में विराजमान, गुरु-मुख से सही रूप में जानने योग्य तथा मूर्खों द्वारा पूर्ण रूप से अज्ञात, दिव्य ज्ञान का उपदेशक तथा परमेश्वर रूप है, उसका ज्ञान फलदायक होता है।
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।। ४८ ।।
जिसकी ईश्वर में परम श्रद्धा है और जैसी श्रद्धा ईश्वर में है वैसी गुरु में भी है, उस महान आत्मा को उक्त अर्थ (दिव्य ज्ञान) अवश्य प्रकाशित करते हैं।
कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लववद्दृढम् ।
अभ्यासवासनाशक्त्या तरन्ति भवसागरम् ।। ४९ ।।
लोग कर्णधार गुरु को पा कर गुरु-वाक्य की सुदृढ नौका पर आरूढ़ हो अभ्यास-धारणा-रूपी शक्ति से संसार सागर को पार करते हैं।
दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् ।
दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना ।। ५० ।।
सदगुरु की दया के बिना विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्त्व-दर्शन करना दुर्लभ है, आत्मैक्य दुर्लभ है।
नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ।
निष्प्रपंचाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ।। ५१ ।।
उस शिव-रूप, सच्चिदानन्द, प्रपंचों से रहित, शान्त, निरालम्ब, तेज- युक्त गुरु को प्रणाम है।
त्वं हि विष्णुर्विरंचिस्त्वं त्वं च देवो महेश्वरः ।
त्वमेव शक्तिरूपोसि निर्गुणस्त्वं सनातनः । । ५२ ।।
तू ही विष्णु है, तू ही ब्रह्मा है और तू ही महेश्वर है। तू ही शक्ति का रूप है। तू ही निर्गुण शाश्वत ब्रह्म है।
नमः शान्तात्मने तुभ्यं नमो गुह्यतमाय च ।
अचिन्त्यायाप्रमेयाय अनादिनिधनाय च ॥५३॥
उस शान्त आत्मन् को प्रणाम है जो रहस्यमय, अचिन्तनीय, अपरिमित और आदि-अन्त से मुक्त है।
नमस्ते सते जगत्कारणाय
नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय ।
नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय
नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ।। ५४ ।।
जगत् के कारण सत् तुझे प्रणाम है। लोकों के आश्रय चित् तुझे प्रणाम है। मुक्ति को प्रदान करने वाले अद्वैत तत्त्व तुझे प्रणाम है। शाश्वत सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म तुझे प्रणाम है।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ।
व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ।।५५ ।।
जो ईश्वर, गुरु, आत्मा — इन तीनों रूपों में प्रकट होता है, जो आकाशवत् रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस दक्षिणामूर्ति को प्रणाम है।
निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् ।
गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ।। ५६ ।।
जो सब विद्याओं के स्रोत हैं, जो संसार से पीड़ितों के लिए वैद्य हैं, जो सभी लोकों के गुरु हैं, उन दक्षिणामूर्ति को प्रणाम है।
सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदम् ।
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोतिनिश्चितम् । । ५७ ।।
यह (गुरु-गीता) सब पापों को हरने वाली है; धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-प्रदायक है। जिस विषय-वस्तु की व्यक्ति इच्छा करता है, इसके माध्यम से प्राप्त करता है। यह निश्चित है।
शुचीभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये ।
तेषां दर्शनसंस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते ।। ५८ ।।
जो निर्मल और ज्ञानवान् हो कर इस गुरु-गीता का पाठ करते हैं, उनके दर्शन एवं स्पर्श मात्र से ही लोग पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं।
ॐ शान्तिः ! शान्तिः!! शान्तिः !!!