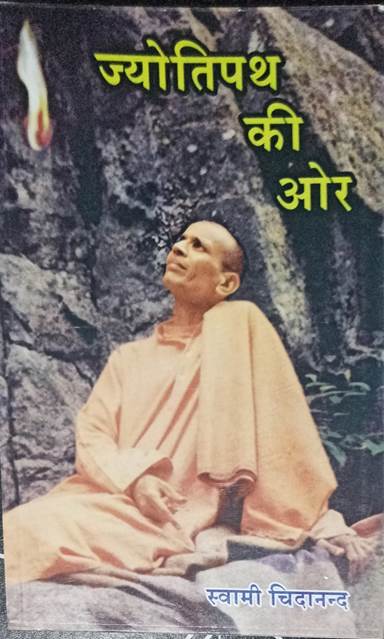
ज्योतिपथ की ओर
GUIDE LINES TO ILLUMINATION
का हिन्दी अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती
अनुवादिका
सुश्री प्रकाश अग्रवाल
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय: शिवानन्दनगर-२४९ १९२
जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dishq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण :१९७६
द्वितीय हिन्दी संस्करण :१९९१
तृतीय हिन्दी संस्करण : २००९
चतुर्थ हिन्दी संस्करण :२०१६
पंचम हिन्दी संस्करण : २०२२
(५०० प्रतियाँ)
• द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
HC 15
PRICE: 125/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा
प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी प्रेस,
पो. शिवानन्दनगर-२४९ १९२, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित ।
For online orders and Catalogue visit: disbooks.org
प्रकाशकीय
जीवन का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप अथवा आत्मा को जान लेना है जिसके जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि भगवान् उसके अन्तर में हैं, वह भगवान् में है और भगवान् उसमें हैं। भगवत्प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य से रहित मानव-जीवन व्यर्थ है, सार-रहित है।
इस अध्यात्म-पथ पर उन्नति करने वालों को आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत तत्त्वों को जानना चाहिए। इस दिशा में प्रस्तुत ग्रन्थ 'ज्योतिपथ की ओर' कुछ व्यावहारिक और उपादेय सूचनाएँ प्रस्तुत करने का उद्देश्य पूरा करता है। इसमें आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत तत्त्व निहित हैं। यह ग्रन्थ परम सत्य के सच्चे जिज्ञासुओं के सेवार्थ तथा मानव मात्र के लिए लाभप्रद अध्यात्म-ज्ञान के प्रसार हेतु सप्रयास है। इस प्रकार के ग्रन्थ प्रायः एक ही विषय-वस्तु पर आधारित होते हैं, परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ 'ज्योतिपथ की ओर' में अध्यात्म-पथ के साधकों के लिए व्यवहारार्थ अनेक उपयोगी संकेत दिये गये हैं जो श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज की सन् १९६९-७० की विदेश यात्रा के दौरान विविध स्थानों पर दिये हुए भाषणों से संकलित किये गये हैं।
-द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पुरोवाक्
मानव-जीवन दुर्लभ उपहार है। यह प्रभु द्वारा दिया गया उपहार है। इस मयं संसार में तीन वस्तुएँ पाना अति कठिन है-मानव जीवन, मोक्ष की कामना- मुमुक्षुत्व तथा सन्तों, ज्ञानियों का संग। ये तीनों ही प्रभु के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही प्राप्त होती हैं। इन तीनों में प्रमुख और प्रथम मनुष्य-जन्म बहुत अधिक मूल्यवान् है। सत्ता की यही अवस्था है जिसमें जीव बुद्धि-सम्पन्न होता है और उसे विवेक-शक्ति, जो अत्यधिक दुर्लभ क्षमता है, प्राप्त होती है। यही कारण है कि मानव-जीवन को ईश्वर का बड़ा ही दुर्लभ उपहार माना गया है।
जीवन का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप अथवा आत्मा को जान लेना है जिसके जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि भगवान् उसके अन्तर में हैं, वह भगवान् में है और भगवान् उसमें हैं। भगवत्प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य से रहित मानव जीवन व्यर्थ है, सार-रहित है।
इस अध्यात्म-पथ पर उन्नति करने वालों को आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत तत्त्वों को जानना चाहिए। इस दिशा में प्रस्तुत ग्रन्थ 'ज्योतिपथ की ओर' कुछ व्यावहारिक और उपादेय सूचनाएँ प्रस्तुत करने का उद्देश्य पूरा करता है। इसमें आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत तत्त्व निहित हैं। यह ग्रन्थ परम सत्य के सच्चे जिज्ञासुओं के सेवार्थ तथा मानव मात्र के लिए लाभप्रद अध्यात्म-ज्ञान के प्रसार हेतु सद्प्रयास है। इस प्रकार के ग्रन्थ प्रायः एक ही विषय-वस्तु पर आधारित होते हैं, परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ 'ज्योतिपथ की ओर' में अध्यात्म-पथ के साधकों के लिए व्यवहारार्थ अनेक उपयोगी संकेत दिये गये हैं जो मेरी सन् १९६९-७० की विदेश यात्रा के दौरान विविध स्थानों पर दिये हुए भाषणों से संकलित किये गये हैं। मैं यह पुस्तक आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत तत्त्वों के जिज्ञासुओं के कर कमलों में अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसके द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।
मैं यह ग्रन्थ पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ जो आज भौतिक रूप में विद्यमान नहीं हैं, परन्तु जिनकी अदृश्य आत्मिक उपस्थिति अब भी मेरा पथ-प्रदर्शन करती रहती है।
-स्वामी चिदानन्द
श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती
(जीवन का एक रेखा-चित्र)
स्वामी चिदानन्द जी के पूर्वाश्रम का नाम श्रीधर राव था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास राव और माता का नाम सरोजिनी था। उनका जन्म २४ सितम्बर, १९१६ को हुआ। वह अपने माता-पिता की पाँच सन्तानों में से द्वितीय सन्तान और उनके पुत्रों में ज्येष्ठ थे। श्रीनिवास राव समृद्ध जमींदार और दक्षिण भारत में कई ग्राम, विस्तृत भूखण्ड और राजसी भवन के स्वामी थे। सरोजिनी देवी एक आदर्श भारतीय माता थीं और अपने साध्वाचार के लिए प्रसिद्ध थीं।
आठ वर्ष की आयु में उनके जीवन पर एक अनन्तैया नामक व्यक्ति का प्रभाव पड़ा। श्री अनन्तैया इनके दादा के मित्र थे और रामायण तथा महाभारत महाकाव्य से इन्हें कथाएँ सुनाया करते थे। तपश्चर्या, ऋषि-जीवन यापन और भगवद्-दर्शन इनके प्रिय आदर्श बने।
इनके फूफा श्रीकृष्ण राव ने इनके चतुर्दिक् व्याप्त भौतिकवादी जगत् के कुप्रभावों से इनकी रक्षा की और इनमें निवृत्ति-जीवन का बीज वपन किया। जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध किया, यह उस बीज को सन्तत्व में विकसित होने तक बड़ी प्रसन्नता से धारण किये रहे।
प्रारम्भिक शिक्षा मैंगलोर में प्राप्त कर यह सन् १९३२ में मद्रास के मुत्थैया चेट्टी स्कूल में प्रविष्ट हुए जहाँ पर एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। इन्होंने अपने प्रफुल्ल व्यक्तित्व, अनुकरणीय व्यवहार तथा असाधारण गुणों से अपने सम्पर्क में आने वाले सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों के हृदय में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया।
सन् १९३६ में लोयोला कालेज में प्रवेश किया, जिसमें बहुत ही मेधावी विद्यार्थी ही प्रवेश पाते हैं। सन् १९३८ में साहित्य-स्नातक (बी. ए.) की उपाधि प्राप्त की। इनका विद्यार्थी-जीवन अधिकांशतः ईसाई कालेज में व्यतीत हुआ, इसका भी अपना महत्त्व है। इनके हृदय में प्रभु ईसा, ईशदूतों तथा ईसाई सन्तों के भव्य आदर्श का हिन्दू-संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट एवं अभिजात तत्त्वों के साथ सुन्दर संश्लेषण हुआ है। बाइबिल का स्वाध्याय इनके लिए केवल दैनिक कृत्य ही नहीं था, वह तो इनके लिए भागवत-जीवन था। वह इनके लिए उतना ही जीवन्त और सत्य था जितना कि वेद, उपनिषद् और गीता के शब्द। अपने स्वाभाविक विशाल दृष्टिकोण के कारण ये कृष्ण में ईसा के, कृष्ण के स्थान में ईसा के नहीं, दर्शन कर सके। यह ईसा मसीह के उतने ही भक्त थे जितने कि भगवान् विष्णु के थे।
राव परिवार उच्च कोटि की सदाचारिता के लिए प्रसिद्ध था और यह श्रीधर राव के जीवन में भी प्रतिष्ठित किया गया। उनके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के कण-कण में दान और सेवा का गुण व्याप्त था। इन सद्गुणों ने श्रीधर राव में अपना साकार रूप ग्रहण किया। उन्होंने इन गुणों की अभिव्यक्ति के साधन ढूँढ़ निकाले। कोई भी व्यक्ति, जो उनसे सहायता की याचना करता था, खाली हाथ वापस नहीं जाता था। वह दरिद्रों को मुक्त हस्त से दान करते थे।
कुष्ठियों की सेवा ने उनके जीवनादर्श का रूप लिया। वह अपने घर के विस्तृत मैदान में उनके लिए झोपड़ियाँ बनवाते और उनकी इस तरह से देखभाल करते मानो वे साक्षात् देवता हों। कालान्तर में जब वह आश्रम में आ गये तो उनके प्रारम्भिक जीवन का यह गुण पूर्ण व निर्बाध रूप से अभिव्यक्त हुआ। 'सभी प्राणी एक हैं', इस परम ज्ञान पर आश्रित दिव्य प्रेम के विशाल साम्राज्य में श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ व्यक्ति भी कदाचित् ही प्रवेश करने का साहस करे। पास-पड़ोस से नाना प्रकार के उग्र व्याधियों से पीड़ित रोगी उनके पास आते और चिदानन्द जी के लिए वे रोगी नहीं थे, साक्षात् नारायण थे। वह मृदु प्रेम और करुणा से उनकी सेवा करते। उनके हाथों की गति ही उनका ऐसा चित्रांकन करती मानो वह साक्षात् भगवान् नारायण की पूजा कर रहे हों। कोई भी कार्य हो, कितनी ही तात्कालिक अविलम्ब्यता का कार्य हो, वह रुग्ण आश्रमवासी को सुख और सान्त्वना देने से कभी न रुकते।
सेवा और विशेषकर रोगियों की सेवा से ऐसा पता चला कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत पृथक् सत्ता का भान नहीं रहता। ऐसा लगता है कि मानो उनका शरीर एक ऐसे जीवात्मा से ढीला-ढाला चिपटा हुआ है जो कि पूर्ण रूप से उद्बुद्ध हो चुका है और यह अनुभव करता है कि वही सब शरीरों में निवास करता है।
और उनकी यह सेवा केवल मानव-जाति तक ही सीमित नहीं थी। पशु और पक्षी भी, यदि मनुष्य से अधिक नहीं तो कम-से-कम मनुष्य के समान उनके ध्यान के अधिकारी थे। वह उनकी पीड़ा की भाषा समझते थे। एक बीमार कुत्ते की सेवा पर गुरुदेव ने उनकी बड़ी सराहना की थी। किसी व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में किसी मूक प्राणी पर नृशंसता का व्यवहार करते देख कर वह अपने हाथ के इंगित से उसे उग्र शिक्षा देते।
कुष्ठियों के कल्याण-कार्य में गम्भीर और स्थिर रुचि रखने के कारण वह राजकीय अधिकारियों की प्रशंसा व विश्वास के पात्र बने और प्रदेश द्वारा संस्थापित कुष्ठी कल्याण समिति के लिए निर्वाचित किये गये। मुनि-की-रेती अधिसूचित क्षेत्र समिति के वह पहले तो उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
यद्यपि श्रीधर सम्पन्न परिवार के थे, तथापि एकान्त और ध्यान में संलग्न रहने के लिए उन्होंने बचपन से ही सभी सांसारिक भोगों को तिलांजलि दे दी। जहाँ तक अध्ययन का सम्बन्ध है, कालेज की पुस्तकों की अपेक्षा आध्यात्मिक पुस्तकों में उनकी अधिक रुचि थी। लोयोला कालेज में रहते हुए भी वह पाठ्य-पुस्तकों की तुलना में आध्यात्मिक पुस्तकों को प्राथमिक स्थान देते थे। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द और गुरुदेव की पुस्तकों को अन्य सभी पुस्तकों से पूर्वता देते थे।
श्रीधर अपने ज्ञान में दूसरों को इतना सहभागी बनाते थे कि वह घर तथा पास-पड़ोस के लोगों के वस्तुतः गुरु बन गये। उनके साथ वह सच्चाई, प्रेम, शुचिता, सेवा और भगवद्-भक्ति की चर्चा किया करते थे। वह श्री राम का जप करने के लिए उन्हें उत्साहित किया करते थे। जब वह बीस वर्ष की वय के ही थे, तभी से उन्होंने नवयुवकों को रामतारक मन्त्र की दीक्षा देना आरम्भ कर दिया था। उनके अनुयायियों में एक श्री योगेश थे जो बालक गुरु श्रीधर द्वारा दिये गये तारक मन्त्र का जप १२ वर्ष तक निरन्तर करते रहे।
वह श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानन्द के परम प्रेमी थे। मद्रास के मठ में नियमित रूप से जाते और वहाँ पूजा में भाग लेते थे। स्वामी विवेकानन्द का संन्यास के लिए आह्वान उनके शुद्ध हृदय में गूँजता रहता था। महानगर में पधारने वाले साधु-सन्तों के दर्शन के लिए वह सदा ही लालायित रहते थे।
सन् १९३६ में श्रीधर छुप कर घर से चले गये। उनके माता-पिता ने बड़ी खोज के बाद उन्हें तिरुपति के पवित्र पर्वतीय मन्दिर से कुछ मील दूर एक धर्मात्मा सन्त के निर्जन आश्रम में पाया। बहुत समझाने-बुझाने पर वे घर वापस गये। उनका यह अस्थायी वियोग परिवार, मित्र और सम्पत्ति के मोहमय संसार से अन्तिम विदाई लेने की तैयारी थी। जब वह घर पर थे, तब भी उनका हृदय अपने अन्तर्वर्ती ज्ञान-गंगा के सनातन प्रणव-नाद के साथ सस्वर हो कर स्पन्दित होता और आध्यात्मिक विचारों के निस्तब्ध वनों में रमण करता रहता था। तिरुपति से वापस आने पर उन्होंने सात वर्ष घर में व्यतीत किये। इन दिनों उनके जीवन पर एकान्तवास, सेवा, आध्यात्मिक साहित्य के गहन अध्ययन, आत्म-संयम, इन्द्रिय-निग्रह, सरल और सात्त्विक जीवनचर्या और आहार, विलासिता का परिहार और तपोनिष्ठ जीवन के अभ्यास की गहरी छाप पड़ी और ये ही उनकी अन्तः आध्यात्मिक शक्ति के संवर्धन में सहायक हुए।
सन् १९४३ में उन्होंने अपने भावी जीवन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया। ऋषिकेश के श्री स्वामी शिवानन्द जी से वे पहले से ही पत्र-व्यवहार कर रहे थे । अन्त में वह आश्रम में सम्मिलित होने के लिए स्वामी जी की अनुमति प्राप्त करने में सफल हुए।
आश्रम में पदार्पण करने के साथ ही उन्होंने स्वभावतः औषधालय का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। उनके हाथों में रोग के निवारण की अद्भुत शक्ति थी। यह ख्याति चारों ओर फैल गयी, जिससे शिवानन्द दातव्य औषधालय में रोगियों का जमघट लगने लग गया।
आश्रम आने के तत्काल बाद ही श्रीधर ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का पर्याप्त परिचय दिया। उन्होंने भाषण दिये, पत्र-पत्रिकाओं के लिए लेख तैयार किये और आश्रम में पधारने वाले जिज्ञासुओं को आध्यात्मिक उपदेश दिये। सन् १९४८ में जब 'योग-वेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय' (अब योग-वेदान्त आरण्य अकादमी के नाम से प्रसिद्ध) की स्थापना हुई, तो गुरुदेव ने उन्हें इसका उप-कुलपति और राजयोग का प्राध्यापक नियुक्त कर यथोचित सम्मान दिया। प्रथम वर्ष में उन्होंने महर्षि पतंजलि के योग-सूत्रों की प्रांजल व्याख्या प्रस्तुत कर जिज्ञासुओं को योग-मार्ग की प्रेरणा दी।
आश्रम में अपने निवास-काल के प्रथम वर्ष में ही उन्होंने स्वामी शिवानन्द जी की अमर जीवन-कथा पर 'Light Fountain' (लाइट् फाउन्टेन) नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ पर गुरुदेव ने एक बार अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था- "ऐसा समय आयेगा जब शिवानन्द इस जगत् से प्रयाण कर जायेगा, किन्तु 'लाइट् फाउन्टेन' सदा अमर रहेगी।"
कार्यबहुल एवं गम्भीर साधनामय जीवन होते हुए भी उन्होंने गुरुदेव के निर्देशन में सन् १९४७ में योग-म्यूज़ियम (योग-कौतुकालय) की स्थापना की जिसमें वेदान्त का सारा दर्शन तथा योग-साधना की सभी प्रक्रियाएँ चित्रों द्वारा दर्शायी गयी हैं।
सन् १९४८ के अन्तिम दिनों में जब श्री निजबोध जी ने दिव्य जीवन संघ के महासचिव के पद से अवकाश ग्रहण किया, तो गुरुदेव ने श्रीधर को उनके स्थान पर मनोनीत किया। अब उनके कन्धों पर संघ की व्यवस्था का महान् उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस नियुक्ति के तत्काल बाद ही इन्होंने संस्था की सभी प्रवृत्तियों में उपस्थित रह कर, मन्त्रणा दे कर तथा बुद्धिमत्तापूर्वक उनका नेतृत्व वहन कर आध्यात्मिकता का पुट दिया। वह सभी को अपनी चेतना को दिव्य चेतना के समकक्ष लाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे।
१० जुलाई १९४९ को गुरु-पूर्णिमा के दिन श्रीधर परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज से दीक्षा ले कर संन्यास-आश्रम में प्रविष्ट हुए। अब वह 'स्वामी चिदानन्द' के नाम से अभिहित हुए। चिदानन्द का अर्थ है-सर्वोपरि चेतना और ज्ञान में स्थित व्यक्ति।
भारत के विभिन्न भागों में दिव्य जीवन संघ की शाखाओं के कुशलतापूर्वक संयोजन का श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सन् १९५० में गुरुदेव की नवयुग निर्माणकारी अखिल भारतीय यात्रा की सफलता में उनका योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से भारत के बड़े-बड़े राजनैतिक तथा सामाजिक नेता गण, राजकीय उच्च पदाधिकारी तथा राज्यों के नरेशों में दिव्य जीवन के अभियान की ओर जाग्रति पैदा की।
गुरुदेव ने स्वामी चिदानन्द को अपने व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में नूतन जगत् में दिव्य जीवन के सन्देश का प्रचार करने के लिए भेजा। उन्होंने अमरीका का यह विस्तृत पर्यटन सन् १९५९ के नवम्बर माह में आरम्भ किया। अमरीकावासियों ने पाश्चात्य वैचारिक भूमि में पले हुए लोगों में भारतीय योग की व्याख्या प्रस्तुत करने में पूर्ण निष्णात भारत के एक योगी के रूप में उनका स्वागत किया। उन्होंने दक्षिणी अमरीका का भी पर्यटन किया और माण्टीवीडियो तथा ब्यूनिस आयर्स आदि नगरों में धर्म-प्रचार किया। अमरीका से उन्होंने यूरोप की क्षिप्र यात्रा की और १९६२ के मार्च माह में आश्रम वापस आ गये।
अप्रैल १९६२ में उन्होंने दक्षिण भारत की तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया। अपनी इस यात्रा में वह दक्षिण के मन्दिरों और तीर्थस्थानों के दर्शन करते तथा आत्मप्रेरक भाषण देते थे। गुरुदेव की महासमाधि से लगभग आठ-दश दिन पूर्व ही वह १९६३ की जुलाई के प्रारम्भ में ही दक्षिण की यात्रा से आश्रम में वापस आ गये। इसे वह एक अलौकिक घटना ही मानते हैं।
अगस्त सन् १९६३ में वह गुरुदेव के उत्तराधिकारी के रूप में दिव्य जीवन संघ के परमाध्यक्ष तथा योग-वेदान्त आरण्य अकादमी के कुलपति निर्वाचित हुए।
महान् गुरु के एक सुयोग्य उत्तराधिकारी होने के नाते उन्होंने इन कतिपय वर्षों में न केवल इस संस्था की सुदूर देशों तक फैली हुई शाखाओं के ढाँचे में ही, वरन् विश्व-भर के उन असंख्य साधकों के हृदयों में भी जो कि उनका परामर्श, उनकी सहायता तथा मार्ग-दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहे हैं-त्याग, सेवा, प्रेम और आध्यात्मिकता का झण्डा ऊँचा बनाये रखने के लिए अथक श्रम किया है। एक उन्नत कोटि के संन्यासी का अनुकरणीय जीवन यापन करने, आध्यात्मिकता का आकर्षण-केन्द्र होने तथा विश्व में दिव्य जीवन के भव्य आदर्शों को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए अपने बहुमुखी उग्र प्रयास के कारण वह सभी लोगों के प्रेम-पात्र बन गये।
पूर्ण अवधानपूर्वक सुरक्षित उनके व्यक्तित्व के स्वभावगत सौजन्य तथा स्वच्छन्द सेवाभावी प्रेमल स्वभाव ने लाखों व्यक्तियों के जीवन में अमित सान्त्वना प्रदान की है। देश के सुदूर और निकट के स्थानों की यात्रा के साथ-साथ स्वामी जी ने अभी हाल ही में मलेशिया तथा हाँगकाँग की यात्रा की और वहाँ पर सच्ची संस्कृति, आध्यात्मिकता तथा सभी कर्मों में अहंभावराहित्य की भावना को विकीर्ण एवं प्रसारित किया और इस भाँति अगणित व्यक्तियों के हृदयों में दिव्य जीवन यापन की कला स्थापित की। उनके इन गुणों के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके प्रति अमित कृतज्ञता का भाव द्योतन करते हैं।
संसार-भर में दिव्य जीवन के महान् आदर्शों के पुनरुज्जीवन के लिए अथक परिश्रम करते-करते २८ अगस्त २००८ को परम आराध्य श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज ब्रह्मलीन हो गये।
विषय-सूची
५. ध्यानोपासना और उसका महत्त्व
१२. शुद्धता : योग-पथ-निर्मात्री
१५. दिव्यता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है; अतः नियमित साधना द्वारा उसे प्रस्फुटित करो.
१६. मन : बन्धन और मोक्ष का कारण
१७. आध्यात्मिक विश्व-गुरु स्वामी शिवानन्द
२०.गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज
२६. स्वाध्याय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव
२७. अलौकिक घटनाएँ और योग में उनका स्थान
२९. योग : महत्त्व और स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता
३१. श्री स्वामी शिवानन्द जी तथा उनका सन्देश
बीस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नियम
१. योग के सिद्धान्त
योग केवल निर्विकल्प समाधि में ही नहीं, प्रत्युत प्रतिक्षण है। मन में कोई विचार आने पर यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते या उसे दमन नहीं करते, तो आप योग में असफल माने जायेंगे। हर विचार और हर कर्म में आपको अपनी वृत्तियों पर नियन्त्रण रखना है। तभी योग का उद्देश्य पूर्ण होगा और आप दिव्य जीवन यापन करेंगे। जानते हैं, इसमें कितनी देर लगती है? केवल एक क्षण। एक सेकेण्ड में चलचित्र फिल्म के कितने चित्र गुजर जाते हैं? मन के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। संस्कारों से ले कर इच्छा-पूर्ति की चेष्टा तक सम्पूर्ण प्रक्रिया एक सेकेण्ड में घट जाती है। अनुभव से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से वासना और वासनाओं से वृत्ति। कल्पना द्वारा वृत्ति इच्छा का रूप ले लेती है। इच्छा से जब अहं का योग होता है, तब वह इच्छा तृष्णा बन जाती है तथा आप इच्छा-पूर्ति के लिए चेष्टा करने को बाध्य होते हैं। मन की यह प्रक्रिया निरन्तर क्रियाशील है।
वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन की खोज में हैं जो सदैव, निरन्तर चलती रहे, कभी न रुके। इस तरह की मशीन की खोज यदि आपको करनी हो, तो वह आपके अन्तर में ही है। उसे मन कहते हैं। इसी का सामना करना है। जितनी भी वासनाएँ और जितने भी संस्कार आपने बनाये हैं, वे सब ज्यों-के-त्यों उसमें हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप एक कार्य कर सकते हैं और वह यह कि आप नये संस्कारों को न बनने दीजिए और न पुराने संस्कारों को नये संस्कारों से सबल ही होने दीजिए। लेकिन यह कैसे सम्भव हो? हम प्रतिदिन अपनी पाँचों ज्ञानेन्द्रियों द्वारा नये अनुभव करते हैं। तब इन अनुभवों को हम कैसे रोकें कि ये मन पर अपने संस्कार न बना सकें? क्या ऐसी कोई विधि है? ये विषय कैसे मन में प्रवेश कर संस्कार बन जाते हैं?
एक विषय है, आप अपनी किसी ज्ञानेन्द्रिय से उसे अनुभव करते हैं। प्रथमतः विषय और ज्ञानेन्द्रिय का संयोग होता है। यही पहली चीज है। इसके उपरान्त क्या घटित होता है? अभी तक तो मानव के बाहरी व्यक्तित्व की कोर ही स्पर्श की गयी है। मान लीजिए, आप किसी कार्य में पूर्णरूपेण दत्तचित्त हैं, आपका भाई या बहन आ कर आपको हाथ से स्पर्श करती है (इन्द्रिय ने विषय स्पर्श किया); परन्तु आपको उसका बोध नहीं हो पाता, क्योंकि आपका मन वहाँ नहीं है। अतः इन्द्रिय इस स्पर्श की अनुभूति को मन तक न पहुँचा सकी।
विषय इन्द्रियों से संयुक्त होते हैं। इन्द्रियाँ उन्हें मन तक पहुँचा देती हैं; परन्तु यदि आप उसमें नहीं हैं अर्थात् आपमें 'मैं' भाव वहाँ नहीं है, तब अपने स्वभाववश मन कैसा भी संस्कार बनाये, आपके लिए कोई महत्त्व नहीं रखता। अतएव यदि अहं न हो तो विषय मन की गहराइयों तक प्रविष्ट नहीं हो पाता। यदि अहं को किसी अन्य विचार में लगा दें, तो इन्द्रियों द्वारा बना हुआ संस्कार कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। परन्तु यदि 'मैं' वहाँ है, तो विषय जा कर आपकी चेतना से टकरायेगा और यदि 'मैं' सजग नहीं है, इस ओर से असावधान है, अज्ञानावस्था में है, सांसारिकता में डूबा है तो वह तुरन्त इन अनुभवों को ग्रहण कर आपमें विषयों के प्रति इच्छा जाग्रत कर देगा।
यदि आपमें विचार-प्रक्रिया को समझने की कमी है और आप सावधान नहीं रहे, तो ज्यों-ही किसी प्रिय वस्तु का विचार आया, आप उसके प्रति आकर्षित हो उसे पाने की इच्छा करने लगेंगे। आप रुपया-पैसा देखते हैं और तुरन्त उसे लेना चाहते हैं। यदि इच्छा यहाँ तक आ जाती है, तब एक ही काम हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं? आप उस इच्छा को जला कर भस्म ही कर सकते हैं और इच्छाओं को भस्म करने के लिए केवल एक ही अग्नि है। वह अग्नि नचिकेता के पास थी। यमराज ने उसके सामने कितने आकर्षक और लोभनीय पदार्थ रखे। उन्होंने धन, सौन्दर्य, बल, शक्ति, राज्य, समस्त भुवनों का स्वामित्व, समस्त विद्याएँ आदि उसे भेंट करनी चाहीं। उन्होंने उसके समक्ष महा-आकर्षक एवं प्रलोभनीय समस्त भुवनों का बड़ा ही विषद वर्णन किया। परन्तु नचिकेता था कि उसने समस्त इच्छाओं को ही भस्म कर दिया था। उसके पास वैसी अग्नि थी और वह अग्नि है 'मुमुक्षुत्व' । मुमुक्षुत्व ही वह असली अग्नि है जिसमें समस्त इच्छाएँ, लालसाएँ डाल कर भस्म की जाती हैं। यही अग्नि दिव्य जीवन यापन करने वाले समस्त साधकों, योगियों और वेदान्तियों का मूलभूत गुण है।
यदि आप दिव्य जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके हृदय में सर्वदा मुमुक्षुत्व की प्रबल आकांक्षा होनी चाहिए और निरन्तर योग की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। ज्वाला अवश्य होनी चाहिए। जीवन की बाह्य पद्धति को आप पूर्णरूपेण नहीं बदल सकते; परन्तु अन्तर में मोक्ष ही की अभिलाषा होनी चाहिए। मुमुक्षुत्व की इस अग्नि को अहर्निश जलते रहना चाहिए-आप जगते हों, सोते हों, अकेले हों या लोगों के साथ हों, ध्यान में हों या कर्मरत हों, यह अनि अनवरत जले। इसे बुझने न दीजिए; बल्कि अपनी सत्ता का एक अविभाज्य अंग बना लीजिए। तभी आपका जीवन दिव्य जीवन होगा।
यदि आपमें यह अग्नि है, तब आप चाहे जो भी कर्म करते हों, चाहे किसी भी स्थान पर रह रहे हों, कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि आप दिव्य जीवन जी रहे हैं। अतः आप इन्द्रियों के दास नहीं हो सकते; परन्तु आपको जानना चाहिए कि आपके सावधान रहते हुए भी यदि कोई विषय आपकी अन्तश्चेतना में प्रवेश करता है, तो आप उसे मुमुक्षुत्व द्वारा किस प्रकार जला देंगे? बाहरी द्वार पर पहुँचने से पूर्व ही आपको उसे जला देना होगा; परन्तु किस विधि से? इसकी दो विधियाँ हैं- प्रथम विधि है: मन को सदा अन्तर्मुख रखें। उसे पूर्णतः बहिर्मुखी कभी नहीं होने दें। अतः जब आप विषय-वस्तुओं के बीच विचरण भी करेंगे, इन्द्रियाँ बाहर नहीं दौड़ेंगी। वे अन्तर्मुखी ही रहेंगी। यह अभ्यास अत्यन्त कठिन है; परन्तु करना है। यह 'प्रत्याहार' है और बहुत आवश्यक है। साधक का आदर्श सदैव इस महत्त्वपूर्ण योग्यता 'प्रत्याहार' को अपनाने का होना चाहिए।
दूसरी चीज है उदासीनता-तटस्थ रहना। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो यह कोई अर्थ नहीं रखता। एक मांसाहारी व्यक्ति बाजार जाता है जहाँ मछली, अण्डा, मुर्गी आदि बिकते हैं। उसके मुँह में पानी भर आता है; परन्तु यदि वह व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी, निरामिष भोजन करने वाला हुआ, तो वे चीजें उसके लिए कोई महत्त्व नहीं रखेंगी; क्योंकि उसकी उनमें कोई रुचि ही नहीं है। इसी भाँति हमें स्वयं में परम सत्ता का सतत चिन्तन और ध्यान करने की अभिवृत्ति उत्पन्न कर लेनी चाहिए; क्योंकि उसी के द्वारा हम जगत् के खोखलेपन से, सांसारिक वस्तुओं की व्यर्थता से तथा सम्पूर्ण सृष्टि की अनित्यता से परिचित हो सकेंगे।
निरन्तर अपने अन्तर में इसी चेतना को बनाये रखने से मन की एक अभिवृत्ति सृजित होती है जिससे कोई भी पदार्थ आपके लिए महत्त्व का नहीं रह जाता, वस्तुएँ आपके समक्ष आती हैं, परन्तु तब भी आपके अन्तर में प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी अवस्था को उदासीनता की अवस्था कहते हैं। केवल आप किसी में रुचि नहीं रखते। जिस वस्तु को आप पसन्द नहीं करते, उसके रहने पर भी आप उसके अस्तित्व से अनजान रह जाते हैं। किसी वस्तु में रुचि न रखने की जो अभिवृत्ति है, उसे विश्वजनीन करना पड़ेगा। विषयों के बीच में रहते समय साधक को उदासीन वृत्ति रखनी होगी और संसार में इस विधि से ही चलना होगा।
मनुष्य की दैनिक गतिविधि ही योग और वेदान्त का सार है। यदि व्यक्ति सोचता है कि किसी बड़े आदर्शवाद को अपना कर वह चाहे जो कर सकता है, कह सकता है, तो यह उसकी भूल है। जिस प्रकार प्रत्येक बूँद से सागर बनता है, इसी प्रकार व्यक्ति का हर एक कार्य उसके चरित्र के निर्माण में योग देता है। लोगों का दैनिक क्रिया-व्यापार ही दिव्य जीवन के, योग और वेदान्त के सार-तत्त्व का निर्माण करता है। यदि व्यक्ति अपने प्रत्येक विचार के प्रति सजग रह कर दैनिक जीवन में दिव्य जीवन के मोटे सिद्धान्तों का पालन करेगा, तो आध्यात्मिक जीवन के आधारभूत तत्त्व स्वतः ही आ जायेंगे।
सत्यता, दया और शुचिता मुख्य गुण हैं जो आपके जीवन के कण-कण में परिव्याप्त होने चाहिए। साधक किसी भी मूल्य पर दिव्य जीवन यापन की छोटी-से-छोटी बात भी नहीं भूल सकता। उसका सम्पूर्ण जीवन, विशेषकर प्रारम्भिक जीवन विनियन्त्रित होना चाहिए। यदि वह सोचता है कि ध्यान करने के साथ ही मनचाहा अन्य कुछ भी कर सकता है, तो वह स्वयं को धोखा दे रहा है। योग कोई खिलौना नहीं है कि उसे ले कर आप खेलने लगें। अतः हर एक कार्य समझदारी से करना चाहिए।
सम्पूर्ण व्यक्तित्व को नियन्त्रित करना होगा, साधना होगा, मध्यम मार्ग अपनाना होगा। जैसा कि अपने एक गीत में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज कहते हैं-"थोड़ा खाओ, थोड़ा पीओ...।" इस गीत को हमें सही अर्थ में समझना होगा। इस गीत के दो भाग हैं। जब वे कहते हैं- 'थोड़ा खाओ, थोड़ा पीओ, थोड़ा बोलो, थोड़ा सोओ', तो उनका आशय संयम से है। इनमें अधिकता नहीं होनी चाहिए। ये आवश्यकता से अधिक नहीं होने चाहिए। गीत की यह पंक्ति इस अर्थ में नहीं है कि इन्हें करना अत्यावश्यक है, बल्कि इस अर्थ में है कि इनमें आप अतिशयता न करें। खाने, पीने आदि का जो प्रवृत्तिमूलक जीवन है, वह कम-से-कम होना चाहिए।
कविता के दूसरे भाग में जब गुरुदेव कहते हैं- 'थोड़ा जप हो, थोड़ा आसनाभ्यास, थोड़ा कीर्तन', तो उसका यह आशय नहीं कि ये कार्य अधिक मात्रा में नहीं होने चाहिए, प्रत्युत दूसरी तरह का है। गुरुदेव ने कहा है कि हर एक कार्य आवश्यक है और आपके जीवन की दैनिक चर्या में हर एक का स्थान होना चाहिए। देह से सम्बन्ध रखने वाले स्थूल कर्म कम-से-कम हों और साधन के उच्च पहलू आपके दैनिक कार्यक्रम में समुचित महत्त्व पायें। स्थूल रूप से आपके लिए दिव्य जीवन या आध्यात्मिक जीवन की यही रूपरेखा है। जप, ध्यान, कीर्तन आदि उसका विधेयात्मक पक्ष है। कठोर संयम का जीवन व्यतीत करते हुए मन और इन्द्रियों की आकांक्षित कामनाएँ यह समझ कर पूरी न करना कि इनके पूर्ण करने से हम अधिकाधिक मन और इन्द्रियों के दास हो जायेंगे-इसका दूसरा पक्ष है। योग-साधना को सार्थक बनाने के लिए सदैव आत्म-नियन्त्रण रखते हुए अन्तर्मुख रहिए तथा शान्त वातावरण में स्वाध्याय कीजिए।
संक्षेप में योग के ये ही आधारभूत तत्त्व हैं।
२. श्रद्धा की आवश्यकता
राजनीति और अर्थनीति के विषयों में मतभेद हो तो समझ में आता है; परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मतभेद होने से आश्चर्य होता है, क्योंकि इसमें तो समस्त साधकों का लक्ष्य समान ही होता है और वह है आत्म-साक्षात्कार। तब विचारों में यह अन्तर किस कारण है? एक कारण तो यह है कि भिन्न-भिन्न साधकों के समक्ष उस आत्यन्तिक सत्य के भिन्न-भिन्न पहलू प्रस्तुत किये गये हैं। मान लीजिए, एक स्वर्ण और चाँदी का खम्भा बनाया गया हो। उसमें एक ओर चाँदी और दूसरी ओर सोना हो। एक ओर से देखने पर खम्भा केवल चाँदी का प्रतीत होगा और दूसरी ओर से देखने पर नितान्त सोने का। दूसरी तरह इसे यों भी स्पष्ट किया जा सकता है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में ग्रहण-क्षमता और समझने की शक्ति भिन्न-भिन्न होती है। प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करता है। अतः अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद आदि साधकों की क्षमता के अनुकूल भिन्न-भिन्न साधना के मार्ग हैं। इसलिए धर्मग्रन्थों में कोई असंगति नहीं है। सभी हमारी श्रद्धा के योग्य हैं। आप एक कण श्रद्धा से ही वह कार्य कर सकते हैं जो देखने में असम्भव लगता है।
श्रद्धा की आवश्यकता कहाँ है? क्या व्यक्ति अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करके वस्तुओं का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता? नहीं कर सकता; क्योंकि अन्तःकरण (मानसिक प्रक्रिया) की अपनी सीमाएँ हैं। सभी महापुरुषों ने-चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के ब्रह्मानुभूति के उपरान्त श्रद्धा पर बल दिया है। वे गलत नहीं कह सकते थे; क्योंकि गलत कहने का उनका कोई प्रयोजन नहीं था। बाहरी पदार्थों के अनुभव में अनुभवकर्ता, अनुभव की क्रिया और अनुभूत विषय-तीन तत्त्व होते हैं। इन तीनों के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। जीवन में ये तीन तत्त्व प्रतिक्षण रहते हैं। परम अनुभव प्राप्त करने के लिए इस त्रिधा तत्त्व को नष्ट करना है, त्रिपुटी-लय को उपलब्ध होना है। उस स्थिति में केवल चेतना ही चेतना शेष रह जाती है; महा अनुभव, परम अनुभव मात्र रह जाता है।
परम का स्वरूप सत्ता है। इसे एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करेंगे। आप किसी जंगल में जाते हैं और एक वृक्ष देखते हैं। वृक्ष है। मान लीजिए कोई लकड़हारा आ कर वृक्ष काट डालता है, तब वह वृक्ष 'लड्डा' कहलाता है। वृक्ष का नाम और रूप बदल गया है; परन्तु अस्तित्व गायब नहीं हुआ। अब वह 'लट्ठा' के नाम और रूप में विद्यमान है। लड्डे को भी यदि चीर कर तख्ते बना लिये जायें, तब लट्टे के स्थान पर तख्ते होंगे; लेकिन मूल सत्ता ज्यों-की-त्यों रहती है। अब लीजिए, इन तख्तों से मेज और कुरसियाँ बना दी जायें, तब तख्ते नहीं रहेंगे, परन्तु उनके स्थान पर मेज और कुरसियाँ होंगी। कुछ वर्षों के उपरान्त कुरसियाँ और मेजें टूट-टूट कर व्यर्थ लकड़ी के टुकड़े मात्र रह जाती हैं, तब मेज और कुरसियों का अस्तित्व नहीं रह जाता। मेज और कुरसियों के इन टुकड़ों को जला दिया जाये, तो राख शेष रह जाती है। अब लकड़ी के स्थान पर राख का अस्तित्व है और यदि राख को भी नष्ट कर दिया जाये, तो वैज्ञानिकों के मत में अणु शेष रह जाते हैं और इस प्रकार सत्ता कायम रहती है। अतः आत्यन्तिक सत्य सत् और नित्य है।
परन्तु सत्य को हम अपने मन और इन्द्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि इनका क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। यदि रात्रि में प्रकाश है तो हम कोई वस्तु देख सकते हैं। यदि अन्धकार हो तो नेत्र होते हुए भी वस्तु हमें दिखायी नहीं दे सकती। अतः नेत्र भी देखने के लिए प्रकाश (बाहरी वस्तु) पर निर्भर करते हैं। लेकिन मान लीजिए, यदि चकाचौंध करने वाला प्रकाश हो तो नेत्र नहीं देख सकेंगे। वे विद्युत् जैसे बहुत अधिक तेज प्रकाश से या तो चौंधियाँ जायेंगे या सदैव के लिए दृष्टिहीन हो जायेंगे।
इसी प्रकार यदि कोई वस्तु परदे में छिपी हो, तो नेत्र उसे नहीं देख पायेंगे। स्फटिक जैसे स्वच्छ काँच के गिलास में जल भरा हो और दूर से देखा जाये, तो यह बताना कठिन होगा कि गिलास में जल है अथवा नहीं। जुकाम होने से आप किसी वस्तु की सुगन्ध नहीं ले सकते। अति-धीमी ध्वनि आप सुन नहीं सकते हैं और तेज ध्वनि आपको बहरा कर सकती है। किसी विचार में मग्न रहते समय आप बाहरी कोलाहल नहीं सुन सकते। दूध कितना ही सुस्वादु हो, तीसरे या चौथे प्याले में आपके लिए स्वाद नहीं रह जायेगा। यदि दूध वस्तुतः स्वादिष्ट होता, तो वह सदैव सुस्वादु लगता। तब क्या कारण है कि चौथे प्याले में उतना स्वाद नहीं आता और पाँचवें प्याले से उलटी आने लगती है? स्पष्टतः आपकी इन्द्रियों का क्षेत्र बड़ा सीमित है। इन्द्रियों द्वारा हम समान रूप से अनुभवों में एकरूपता नहीं पाते। पहले दिन आपने भोजन में कौन-कौन से पदार्थ खाये थे, आपको याद नहीं रह सकता। न आप अतीत को याद रख सकते हैं और न भविष्य के लिए कथन कर सकते हैं।
व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान् क्यों न हो, मस्तिष्क में थोड़ी-सी भी खराबी हो जाने पर या उसे किसी मनश्चिकित्सक के पास परामर्श हेतु जाना पड़ेगा अथवा किसी पागलखाने में। मनुष्य की चेतना लुप्त करने के लिए अफीम की एक मात्रा पर्याप्त है। ऐसी हैं ये मन और इन्द्रियों की सीमाएँ! यही नहीं; ईर्ष्या, क्रोध, दुराग्रह, उत्साहहीनता- ये सभी व्यक्ति की दृष्टि को धूमिल कर देते हैं। यदि वह प्रसन्न है तो उसे प्रत्येक वस्तु सुन्दर दिखायी पड़ती है, अन्यथा सभी वस्तुएँ भद्दी, कुरूप। यदि किसी व्यक्ति के मन में द्वेष है, तो सब उसके शत्रु बन जाते हैं। यदि उसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, तो सभी उसके मित्र बन जायेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन द्वारा प्राप्त ज्ञान निर्भर करने योग्य नहीं होता।
हमारे महान् चिन्तकों और मनीषियों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि जो-कुछ हम देखते हैं, वह वस्तु की बाह्य दिखावट है, उसका सत्त्व नहीं है। कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए। आपके अनुसार वह कपड़े का एक टुकड़ा है। आप उसके ताने-बाने के धागे निकाल दीजिए। अब क्या रहा? केवल धागों का ढेर! जैसे पहले वह कपड़ा था, वैसा कपड़ा अब वह नहीं रहा। अब उसे धागों का ढेर कह सकते हैं। इन्हीं धागों को रूई में बदल सकते हैं और रूई को अणुओं में। अतः वस्तुतः देखा जाये तो हम अणुओं को धारण किये हुए हैं।
तो क्या बुद्धि और इन्द्रियाँ किंचित् भी उपयोगी नहीं हैं? निश्चय ही उपयोगी है, किन्तु कुछ सीमा तक। जिस सीमा तक बुद्धि उपयोगी है, उस सीमा तक पहुँचने के उपरान्त वह उपयोगी नहीं रह जाती; बाधक बन जाती है। अतः तब उसे त्याग देना चाहिए। वेदान्त में भी जो मुख्यतः अनवरत जिज्ञासा और व्यतिरेक (विश्लेषण) की प्रक्रिया है, ध्यान के स्तर पर-मन को अन्तर्मुख करने की अवस्था में बुद्धि से बचाव करना पड़ता है। हमारे महामनीषी जानते थे कि मन मनुष्य का आवश्यक अंग नहीं है; अतः उन्होंने मन और बुद्धि को ठुकरा कर एकदम अविज्ञात में छलांग लगा दी। उन्होंने परम सत्य का अपरोक्ष अनुभव किया था और परमानन्द को प्राप्त किया था। इसी को वे दूसरों को बाँटना चाहते थे, इसमें दूसरों को भागीदार बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने कहा- "साधको! चले आओ। हम तुम्हें मोक्ष का मार्ग बतायेंगे जहाँ नित्य आनन्द और स्थायी शान्ति है!" अतः उनके वचनों में विश्वास करना अन्धश्रद्धा नहीं है।
आत्मा के प्रति आत्मा की स्वीकृति श्रद्धा है। मानव की आत्यन्तिक सत्ता अनन्त के अनुसार कार्यशील है। श्रद्धा का उद्भव मन और इन्द्रियों द्वारा नहीं होता। श्रद्धा तो मनुष्य के अन्तरतम की परम सत्ता का स्वभाव है। श्रद्धा शक्ति है। यह महान् आदि-शक्ति है जो मानव का उत्थान कर उसे अलौकिक, इन्द्रियातीत अनुभव में ले जाती है।
महामनीषी आचार्य शंकर ने भी साधन-चतुष्टय की षट्-सम्पत् में श्रद्धा को सम्मिलित किया है। साधन-चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, षटू-सम्पत् (शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान) तथा मुमुक्षुत्व हैं। यदि सभी कुछ जिज्ञासा और विश्लेषण से बोधगम्य हो सकता, तो श्रद्धा को भी अनिवार्य तत्त्व बताने की उन्हें क्या आवश्यकता थी? श्रद्धा के बिना साधक श्रवण तक का अभ्यास नहीं कर सकता। यदि गुरु में उसकी श्रद्धा नहीं है और गुरु-वचन को सन्दिग्ध समझता है, तो वह कैसे कुछ सीख सकता है? इतना ही नहीं, श्रद्धा तो हमारे दैनिक जीवन में भी अपरिहार्य है।
कोई भोजन बनाता है, हम भोजन करते हैं। हमें यह सन्देह नहीं होता कि बनाने वाले ने उसमें विष मिला दिया होगा। हम औषधि के लिए चिकित्सक के पास जाते हैं और उसकी दी हुई औषधि का सेवन करते हैं। उस समय हम यह सन्देह नहीं करते कि उसने औषधि के स्थान पर विष दे दिया होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। हमारे प्राचीन महर्षियों ने परम सत्य की गहराइयाँ जाँची थीं और अपने अनुभव प्रदान किये थे। हम उनकी बात में विश्वास करते हैं जो यह कहते हैं कि वे चन्द्रमा पर गये थे। इसी प्रकार उनके वचनों में भी विश्वास करना उचित है जिन्होंने सत्य के दर्शन किये हैं और जो कहते हैं-"हमने सत्य का अनुभव किया है, उसी प्रकार तुम भी कर सकते हो; परन्तु शर्त है कि सत्य का अनुभव प्राप्त करने के लिए जैसा हमने किया है, वैसा तुम भी करो। प्रयोग करके देखो कि तुम्हें वैसी सफलता प्राप्त होती है कि नहीं।" सन्त हमें आश्वासन देते हैं कि सम्यक् आत्म-विश्लेषण द्वारा हम भी परम सत्य का अनुभव कर सकेंगे।
तुलसीदास कहते हैं कि श्रद्धा रानी की अन्तरंग सखी के समान है। रानी का दर्शन चाहने वाले को जिस महल के अन्तर-कक्ष में रानी रहती है, वहाँ तक कोई सेवक नहीं ले जा सकता। वह केवल अन्तःपुर की ड्योढ़ी तक ले जा सकता है। तदुपरान्त रानी की कोई अन्तरंग सखी ही उसे रानी तक पहुँचाती है। तर्क, पुस्तकीय ज्ञान आदि हमें एक निश्चित सोपान तक ले जाते हैं। उसके परे वे हमारी सहायता नहीं कर सकते, केवल श्रद्धा कर सकती है। वह हमें चरम अनुभव में ले जा सकती है। साधक चाहे राजयोगी हो, चाहे भक्तियोगी अथवा ज्ञानयोगी हो-श्रद्धा-भाव आवश्यक है। भगवान् आपको दिव्य आनन्द के प्रति महान् श्रद्धा प्रदान करें!
३. दिव्य जीवन यापन की कला
जीवन अमूल्य है, दुर्लभ है। जीवन को केवल, दुःख, भग्नाशा, निराशा और भ्रम-जाल न मानिए। इन सब क्षणिक रूपों के साथ ही उसका एक महान् और महिमामय पक्ष रह जाता है और वह यह है कि जीवन सदैव हमारी उच्चतर नियति की ओर चलने का हमें आह्वान देता है और वह उच्चतर नियति है नित्य धाम, अमर पद पा लेना। ईश्वर में परमानन्द का अनुभव कर लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। ईश्वर की ही सत्ता है और वही एक सत् है। वह हमारे जीवन की धुरी है तथा हमारे जीवन का परम ध्येय है। जीवन-सत्ता के लिए, शान्ति और सुख के लिए तथा अपने परम कल्याण के लिए ईश्वर के समान और कोई भी नितान्त अपरिहार्य नहीं है। ईश्वर ही हमारा लक्ष्य है।
जिस पृथ्वी-लोक से हो कर हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, हमें उसमें ही लिप्त हो कर नहीं रहना है, प्रत्युत इस जीवन का उपयोग ईश्वर तक पहुँचने में, उससे एक होने में, उसमें एक होने की अनिर्वचनीय अनुभूति प्राप्त करने तथा उसमें आनन्दमय स्वरूप की झलक पाने में करना चाहिए। यही महाकार्य है। जीवन का प्रमुख व्यापार यही है। छोटी-बड़ी अनेकानेक चीजों के बीच में यही एक महान् वस्तु है जिसे हमें उपलब्ध करना है। अन्य समस्त क्षुद्र वस्तुएँ निरन्तर परिवर्तनशील हैं, बदलती रहती हैं और समाप्त हो जाती हैं; परन्तु जीवन का यह महाव्यापार पालने से आरम्भ हो कर चिता में रखते समय तक भी पूर्ण नहीं होता, हो ही नहीं सकता। यह तो तभी पूरा होगा, जब 'उसे' पा लेंगे। इसके लिए चाहे कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़ें। अनेकानेक विक्षेपों के बीच जीवन का यही मुख्य और महाव्यापार है।
हमारी वर्तमान चेतनावस्था अज्ञान की उपज है। अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण ही जन्म, मृत्यु, पीड़ा और यातना है। यह अहं-भावना कि 'मैं मनुष्य हूँ', 'मैं दुर्बल प्राणी हूँ', 'मैं दोषों और त्रुटियों से पूर्ण हूँ', मूल अज्ञान और कष्टों की बहुप्रज जड़ है। इसी से कामनाएँ अंकुरित होती हैं। कामनाएँ अज्ञान-जनित होती हैं। राग-द्वेष भी अज्ञान-जनित हैं। सांसारिक जीवन में आसक्ति भी अज्ञानवश होती है तथा अपनी अमर आत्मा के स्वरूप का, शाश्वत भागवत जीवन का, नित्य आनन्द की महा-नियति का अनुभव न होना भी अज्ञानवशात् ही है।
देहाध्यास-देह को ही आत्मवत् समझ लेना-मानव की बहुत बड़ी भूल है। अशुद्ध, जड़ और नश्वर देह को शुद्ध अमर आत्मा समझ लेना सांसारिक जीवन की वस्तुतः महान् व्याधि है। अहं, राग, द्वेष, लालसाएँ, तृष्णाएँ, वृत्तियाँ आदि इसी मूल त्रुटि के विकार हैं। इसी मूल त्रुटि से ही अनेक प्रकार की इच्छाएँ तथा उनके अनेक रूप-रूपान्तर पैदा होते हैं। इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु व्यक्ति कर्म करता है। कुछ वस्तुओं को वह पसन्द करता है, कुछ हो नापसन्द करता है, अपने कर्म का फल चाहता है, फल भी प्रायः उसकी इच्छानुरूप नहीं होता और इस प्रकार वह जन्म-मरण के चक्र से बँधा रहता है।
परम दिव्य ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, तब दुःख, कष्ट और यातनाओं का अन्त हो जायेगा, आप अमर आनन्द, शाश्वत शान्ति और अखण्ड सुख प्राप्त करेंगे तथा जन्म-मृत्यु के पाश से एकदम मुक्त हो जायेंगे। विवेक, वैराग्य, उपरति, शम, दम, तितिक्षा, त्याग, श्रद्धा और भक्ति, विश्व-प्रेम, साहस, नम्रता, सत्यवादिता, दया, एकाग्रता तथा ध्यान और मोक्ष की ज्वलन्त आकांक्षा-ये सब आत्म-साक्षात्कार के, ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति के साधन हैं।
ईश्वर स्वयम्भू है। अपने अस्तित्व के लिए वह किसी पर निर्भर नहीं है। वह स्वयंप्रकाश, स्वयंज्योति है। उसे स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। वह दिव्य प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है। उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप हैं, इसके लिए आपको कोई प्रमाण नहीं चाहिए। आपको इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति आये और आपको आपके अस्तित्व के होने का प्रमाण दे। आपके लिए आपका अस्तित्व स्वतः सिद्ध है; परन्तु उसका बाहरी प्रदर्शन नहीं हो सकता। आपकी सत्ता है; अतः आप हैं। ईश्वर को प्रमाण नहीं चाहिए; क्योंकि वह समस्त सत्ताओं का मूल है। उसके होने से ही अन्य सत्ताएँ सम्भव हैं। आप भी इसीलिए हैं; क्योंकि 'वह' है। ईश्वर है, अतः आपका होना भी सम्भव हो गया। विशुद्ध सत्ता के रूप में वह आपके अन्तर में है। वह सब प्रमार्णो का प्रमाण है। वह स्वयं पूर्ण है। सब उसमें हैं। अखिल विश्व, त्रिभुवन उसी में है। वह स्वयं का ज्ञाता स्वयं है।
आजकल सगुण और निर्गुण को ले कर बड़े वाद-विवाद होते हैं। वह ऐसा हो या वैसा हो, यह कहने वाले हम कौन होते हैं? एक मानव ईश्वर को कैसे आदेश दे सकता है कि उसे कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं? हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। यह व्यर्थ है। सगुण हो या निर्गुण, हमें क्या प्रयोजन? हमारे लिए वह सगुण है। दार्शनिकों के लिए, तत्त्वचिन्तकों के लिए, रहस्यवादियों के लिए वह निर्गुण (निरपेक्ष) हो सकता है। हमें इससे कुछ प्रयोजन नहीं। हम साधकों के लिए, हममें से प्रत्येक के लिए वह नितान्त सापेक्ष है। वह हमारे बहुत निकट है।
हम तो इतना भी नहीं जानते कि हमारे अन्तर में क्या हो रहा है? नहीं जानते कि भोजन किस प्रक्रिया से हजम हो रहा है, शिराओं में रक्त कैसे संचरित हो रहा है? हम नहीं जानते कि कलिका किस प्रकार पुष्प में प्रस्फुटित हो जाती है? इस पर भी हम कहते हैं कि हम ईश्वर का स्वरूप जानते हैं-और वे कैसे हों, इसके लिए उन्हें आदेश देने को तत्पर हैं। हमें तो उन्हें केवल प्रेम करना है, केवल उन्हें जानने का प्रयास करना है, केवल उनके पास पहुँचना है, उनकी समीपता पाने को, उनका अनुभव करने को और उन्हीं की सत्ता में प्रविष्ट होने को जीना है। यह महान् लक्ष्य है। यही एक कार्य है जो करणीय है।
हम उनके स्वभाव के सम्बन्ध में बात न करें। हमारे लिए इतना जानना ही पर्याप्त है कि वह अनिर्वचनीय माधुर्य है, आनन्द है, ऐसा आनन्द जो आपकी कल्पना से सर्वथा परे है। कल्पना उसको ग्रहण करने में असमर्थ है। वह आनन्द है, शान्ति है-अद्भुत शान्ति। निश्चल हो जाइए और उस शान्ति का अनुभव कीजिए।
शान्ति का उद्गम वही है। मनुष्य अधिक-से-अधिक जिस आनन्द की कल्पना कर सकता है, वह आनन्द इस असीम का किंचित् हलका-सा प्रतिबिम्ब है। वही आनन्द है। वह सौन्दयाँ का महान् सौन्दर्य और प्रकाशों का परम दिव्य प्रकाश है। वह नित्य अनन्त प्रकाश है, परिवर्तनहीन प्रकाश है। शान्ति, आनन्द, दिव्यता, प्रकाश, शाश्वत सत्ता-सब वही है। वह परम पूर्णता है। इन सबसे अधिक सभी से अधिक-वह हमारा अपना है। वही आपका अपना है। उसकी उपलब्धि हेतु संसार की सभी वस्तुओं से आपको सम्बन्धों का अन्त कर देना है।
चर्चा बहुत हो चुकी है। अच्छा होगा, अब चर्चा या बहस और न करें। यह जानने का प्रयत्न करें कि भगवान हमारा अपना है, इस क्षण भी है, यहीं है। समय बीत रहा है। जीवन अल्प है। हमें अज्ञान की ग्रन्थि को काट कर ब्रह्मानन्द का अनुभव करना है। हमने यहाँ इसीलिए जन्म लिया है। स्वामी शिवानन्द जी के समान पूर्व और पश्चिम के महान् सन्त तथा गुरु जन आपको उस आदि स्रोत तक पहुँचाने के लिए ही आते हैं। ज्ञान का सूर्य आपकी चेतना में उदित हो जाये, वे इसी का प्रयत्न करते हैं। वे आपको उस महा-महिमान्वित गन्तव्य की ओर ले जाने के लिए ही आते हैं। अतः प्रेमी हृदय बनो। सन्तों का स्मरण करो। सबकी सेवा करो। सबमें भगवान् के दर्शन करो। वह अन्तर्यामी ही केवल सत्य है। वह आनन्दमय है। हमें अपने इस अपूर्ण असन्तोषजनक पार्थिव जीवन के माध्यम से ही किसी-न-किसी प्रकार 'उस' तक जाने का मार्ग खोजना है। इन्द्रियों पर अनुशासन रखो। नेत्रों पर अनुशासन रखो। जिह्वा पर अनुशासन रखो। अल्प भोजन करो। अपनी स्वादेन्द्रिय पर संयम रखो, निद्रा कम करो और स्वयं को भगवच्चिन्तन से ओत-प्रोत कर लो। प्रेम से ओत-प्रोत कर लो।
अपनी क्षुद्र द्वेष-भावना को, पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रहों और परस्पर अलगाव की भावना को जीत लो और स्वयं को सबके हेतु प्रेम का, एकता का, कल्याण का सागर बना दो। जाति, धर्म, सम्प्रदाय या इस प्रकार के अन्य अवरोधों में कोई अन्तर न देखो। अपने विश्व-प्रेम की भुजाओं में अखिल ब्रह्माण्ड को समेट लो। स्वार्थपरता त्याग दो, क्रोध पर संयम रखो और सद्गुणों का विकास करो। जब तक यह जीवन है, कुछ अच्छा काम करो, ठोस काम करो। शरीर में जब तक श्वास है, प्रभु से प्रार्थना करते रहो और उसकी कृपा प्राप्त कर इस यात्रा को शीघ्र ही समाप्त करके नित्य आनन्द में, प्रभु में निवास करो। तब ही जीवन सार्थक होता है।
प्रभु की आप पर असीम कृपा हो!
४. धर्म : जीवन का सार-तत्त्व
जीवन के नैतिक मान की परिपूर्ति के लिए धर्म कर्तव्य है, सदाचरण है तथा सद्गुणी जीवन है। वह जीवन का आधार है, जीवन का रक्षक है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जब आप धार्मिक जीवन यापन करेंगे, तो भगवान् आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जायेंगे। धर्म अमर आनन्द की ओर ले जाता है। जहाँ धर्म है वहाँ सफलता है, आनन्द है और शान्ति है। धर्म एक विलक्षण संकल्पना है। वह आदर्श है-आदर्शवाद का जीवन-जो सम्भाव्य है। जीवन को जैसा होना चाहिए, उसका आदर्श है। यह प्राकृतिक विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान पर आधारित न हो कर आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित वास्तविक विज्ञान है। कोई भी व्यक्ति दुःखी नहीं होना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। अशान्ति, भय, अस्थिरता, चिन्ता, परेशानी कोई नहीं चाहता। सब सुख की अनुभूति चाहते हैं। हर एक शान्ति खोजता है। परन्तु शायद ही कोई जानता हो कि सुख और शान्ति दोनों एक हैं और अपृथक् हैं। कदाचित् ही किसी को ज्ञात हो कि इन दोनों का सम्बन्ध वर्णनातीत है।
वह कौन-सा सम्बन्ध है?
सुख पूर्णरूपेण शान्ति पर आश्रित है। शान्ति सुख का कारण है। बिना शान्ति के आप सुख नहीं पा सकते। शान्ति पहले आती है। सुख उसका स्वतः परिणाम है। धूप या अगरबत्ती जलने पर सुगन्ध अनुभव होती है। पुष्प के मुकुलित होते ही उसकी भीनी सुगन्ध आने लगती है। सुख शान्ति का परिणाम है। शान्ति, मन की शान्ति के बिना आपको सुख नहीं मिलेगा। बिना सुख के आप शान्ति तो पा सकते हैं; क्योंकि जिस समय आप पूर्णतः शान्ति की अवस्था में रहते हैं, आप सुख का ध्यान नहीं करते। उस समय सुख हो या न हो, आपके लिए कुछ अर्थ नहीं रखता; क्योंकि सूक्ष्म विश्लेषण करने पर शान्ति का अर्थ ही परमानन्द है। आपके पास यदि एक पात्र भर के शहद है, तो आप मिठास की चिन्ता नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि आपमें सच्ची शान्ति है, तो सुख आपके लिए अनावश्यक हो जाता है; क्योंकि सुख का मूल-तत्त्व शान्ति में पहले से ही है, जिस प्रकार मधुरता का मूल-तत्त्व मधु में है।
जो इस तत्त्व के ज्ञाता हैं, वे कहते हैं- "शान्ति परम लक्ष्य है।" परन्तु जिस शान्ति की वे बातें करते हैं, वह केवल कोलाहल के अभाव से उत्पन्न शान्ति नहीं है, प्रत्युत अनुभव की वह सुनिश्चित अवस्था है जिसमें कोलाहल और तोड़-फोड़ होते हुए भी शान्ति विराजमान रहती है। उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता, भंग नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। इसी कारण वे इसे असाधारण, अद्भुत शान्ति कहते हैं-ऐसी शान्ति जिसे मानव-बुद्धि नहीं समझ सकती, जो मनसातीत है। वही शान्ति है जो दुःख, कष्ट, परेशानियों, निराशा और असफलता के बीच में भी अक्षुण्ण बनी रहती है। चाहे जनता आपसे घृणा करे, मित्र आपका संग छोड़ दें, अपशब्द कहने लगें, यहाँ तक कि चाहे वे आपको क्लेश भी दें-आपमें पूर्ण शान्ति रहेगी। यह अपूर्व असाधारण शान्ति उस समय आती है, जब आप आन्तरिक सत्ता, परम सत्ता का अनुभव करते हैं। इस शान्ति को कोई नहीं छू सकता। कुछ शहीदों में भी यही शान्ति व्याप्त थी। उन्होंने कहा था- "हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो; क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।" और वे उनके लिए भी प्रार्थना कर सके थे जो उन्हें विनष्ट करने पर तुले थे; क्योंकि उनके अन्तर में परमेश्वर की अपार शान्ति थी।
यह शान्ति बुद्धि का अतिक्रमण कर जाती है। इस पर विश्व की कोई शक्ति हावी नहीं हो सकती, प्रभाव नहीं डाल सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। यहाँ तक कि इसका कण मात्र भी ले नहीं सकती; क्योंकि यह शान्ति ही एकमात्र सत् है। यह शान्ति अनुभव की सशक्त सत्तात्मक स्थिति है। यदि आपमें यह शान्ति है तो आप सम्राटों के भी सम्राट् हैं, एक अरबपति भी आपके सामने कुछ नहीं है। यदि आपमें यह शान्ति है तो अखिल विश्व की सम्पदा आपके लिए धूलि के समान है। यही शान्ति हमारा लक्ष्य है। मोक्ष, निर्वाण, ज्ञानोदय, इन्द्रियातीत अनुभव और कुछ नहीं, यह महा-शान्ति ही है।
इच्छाओं का, भ्रम का अन्त हो जाता है। न अशान्ति, न लालसा, कुछ नहीं रह जाती। आप पूर्ण हो जाते हैं। आप दिव्यता से परिपूर्ण, शान्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। परम सत्य ही परम शान्ति है और परम शान्ति ही परमानन्द है। यही उपनिषद् का ब्रह्मानन्द है। यही परम ब्रह्म है, परम 'ताओ' है जो अनिर्वचनीय है और जिसे पाने के उपरान्त कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। यह ऐसी अवस्था है जो अद्वितीय है, अमूल्य है और यह निर्विकार मन से ही सम्भव हो सकती है। जहाँ अनन्त इच्छाओं, विचारों, महत्त्वाकांक्षाओं और विचित्र मोह-जाल के कारण मन चंचल है-उससे शान्ति कोसों दूर है। यदि आप सोचते हैं कि चलो इस इच्छा को पूरी कर लें तो कुछ शान्ति मिले, तो आप पूर्णरूपेण भ्रम में हैं।
इच्छा-तुष्टि का एक ही परिणाम होता है। वह आपकी इच्छा को और बलवती कर देगी; क्योंकि इच्छा माया की एक बड़ी रहस्यमयी विचित्र शक्ति है। वह तुष्टि द्वारा समाप्त नहीं होती। उसका तो अतिक्रमण करके, जीत करके अथवा उच्च लक्ष्य के प्रति उदात्त करके शमन करना है। हर इच्छा के उदित होते ही आप उसे पूर्ण करना चाहने लगें, तो आप भयंकर भूल कर रहे हैं। आप प्रकाश-पथ पर नहीं चल रहे हैं। कुछ ही समय के उपरान्त आपको यह कटु अनुभव होगा कि आप अन्तहीन बन्धन में जकड़ गये हैं। प्रवाह के साथ अनुकूल गति में सन्तरण करना प्रश्न का उत्तर नहीं है। इच्छाओं की इस समस्या का यह समाधान नहीं है। प्रवाह के साथ बहने में आप शीघ्र ही भँवर में फँस जायेंगे। उसमें से निकलने में आपकी केवल आत्म-संयम की शक्ति ही सहायक हो सकती है।
आपको अपनी उच्च प्रकृति को सामने लाना होगा। निम्न प्रकृति को तो सभी कोई छूट दे सकते हैं। संसार के कारागार ऐसे व्यक्तियों से भरे पड़े हैं जिन्होंने अपनी निम्न प्रकृति को खुली छूट दी है। यह नगण्य है-कुछ नहीं ले सकती। जब कभी इच्छा उत्पन्न हो, तुरन्त उसमें चले जाओ। मानव अव्यवस्थित (Chaos) नहीं है, अनगढ़ रचना नहीं है। वह तो ईश्वर की अनुकृति है। इच्छा मन का रोग है। यह जीवात्मा के लिए अभिशाप है। यह भ्रमित अहं की,
मिथ्या मानव-व्यक्तित्व की वेदना है। इच्छा माया है और माया इच्छा है। आपको इसे जीतना है—यही सम्पूर्ण योग का, दर्शन का, ऋषि-महात्माओं के वचनों का सार है। इसे जीतिए। वीरतापूर्वक इस इच्छारूपी भयानक शत्रु को जीत लीजिए। यह बड़ा ही भयानक शत्रु है। इसे जीतने के लिए विशेष शक्ति की अपेक्षा है। इच्छाओं में बह जाना दुर्बलता है; अतः इन्हें रोकिए, इन पर विजय पाइए। यही योग है, यही अध्यात्म है, यही आन्तरिक शक्ति है, यही व्यक्तित्व है और यही वास्तविक सत्य है। आप अपने को दृढ़तापूर्वक स्थापित कीजिए। मन अपना सिक्का जमाता है, इन्द्रियाँ अपना और बुद्धिभ्रंश अपना, तब आप ही क्यों रह जाते हैं? आप अपने को दृढ़ता से स्थापित कीजिए, अन्यथा आप जाल में फँस जायेंगे। आप इनसे भिन्न हैं, सर्वथा भिन्न।
हमारे प्रिय गुरुदेव गाते थे- “तुम न यह शरीर हो, न यह मन हो। तुम अमृत हो, अमर आत्मा हो।" अहर्निश इस महान् सत्य का सहारा लीजिए। इसी ज्ञान का आधार लीजिए। इस आध्यात्मिक ज्ञान से बाल-भर भी इधर-उधर न होइए। सदैव सजग रहिए। इन्द्रियों के, मन के तथा बुद्धि के जाल में मत फँसिए। इच्छाएँ रजस् और तमस् के मिश्रण का परिणाम हैं। जब तक इच्छाएँ आपके मन पर शासन करती रहेंगी, इन्द्रियाँ आपको कठपुतली की तरह नचाती रहेंगी और आप मन की शान्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे; क्योंकि उस समय आपका मन रजोगुण और तमोगुण से भर जाता है।
अतः इस नियम को समझ लीजिए कि मन में सच्ची शान्ति तभी आयेगी जब वह अपने में ही शान्त हो गया होगा, विशुद्ध और सूक्ष्म हो गया होगा और उसके इच्छास्वरूप, इन्द्रियस्वरूप-राजसिक और तामसिक गुण धुल गये होंगे। जहाँ सत्त्व है, वहाँ मानसिक शुद्धता भी होती है। मन के शुद्ध और सूक्ष्म हो जाने पर शान्ति आती है। इसी शान्ति में आनन्द, परम सत्, ब्रह्मभावना का विकास-आरोहण होता है। धर्म जीवन की, आत्म-नियन्त्रित जीवन की, अनुशासित जीवन की, विवेक और त्याग के जीवन की, धर्माचरित संयमित जीवन की, सादे, पवित्र और वासना-रहित जीवन की एक आचरण-पद्धति बनाता है। यही धर्म का सार है। इसी कारण धर्म जीवन की शक्ति और भगवत्साक्षात्कार का साधन बन जाता है।
५. ध्यानोपासना और उसका महत्त्व
आध्यात्मिक जीवन की नींव डाल देने के पश्चात् जब इन्द्रियों के अप्रतिहत आकर्षण पर विजय पा कर व्यक्ति उनका स्वामी हो जाता है, जब सच्चे विवेक और जिज्ञासा द्वारा मानव की आकांक्षित वस्तुओं के नितान्त खोखलेपन को जान कर दृश्य वस्तुओं की ओर उन्मुख अपनी मानसिक वृत्तियों को वश में करके उन्हें नाम और रूप विषयक कामनाओं, वस्तुओं और अनुभवों के प्रति आसक्ति से पूर्णरूपेण विमुख कर लेता है, जब वह बाह्य पदार्थों से अपने मन के प्रत्याहरण की प्रविधि जान लेता है और जब वह अपने अन्तर में शान्ति, समता एवं स्थिरता की अवस्था उत्पन्न कर उसका विकास कर लेता है, तब आखिर में अन्तिम साधन-प्रक्रिया ध्यान की आती है। धर्म में दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित हो जाने की दशा में, पूर्णतः इन्द्रिय-संयम एवं आत्म-नियन्त्रण कर लेने की दशा में, कामनाओं पर विजय पाने तथा आवेगों पर अधिकार कर लेने की दशा में, प्रबुद्ध हो जाने की दशा में तथा आन्तरिक स्थिरता और समता की दशा में आपकी सत्ता सिमट कर सत्य के प्रति बनी आपकी धारणा की ओर गतिशील होने लगती है। आपकी समग्र सत्ता का इस प्रकार सिमटना और अन्तर में सिमटी हुई शक्ति को एक विशिष्ट अभीष्ट दिशा की ओर केन्द्रित करना-आपकी ध्यानोपासना तथा अन्तर्मुख आपकी सत्ता की समग्रता को विशेष दिशा की ओर अविरल एवं अखण्ड गति में बनाये रखने का विषय है।
जब आपकी अन्तर्मुखी वृत्ति की गति तैलधारावत् अविरल और अखण्ड हो जाती है, तब आप ध्यानावस्था में होते हैं। अतः यह आपकी समग्र सत्ता की-अन्तर्मुखी एकीकृत सत्ता की अभीष्ट लक्ष्य की ओर अनवरत सफल गति है। इसे ही ध्यान कहते हैं। इससे इतर ध्यान-सम्बन्धी जो-कुछ है, धारणा है। वह सब लोगों की मनगढ़न्त है। आपके विचार से वह ध्यान है, परन्तु वह ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए पूर्णरूपेण धर्मनिष्ठता की अपेक्षा है। धर्म (Virtue) वे आध्यात्मिक गुण हैं जो ध्यानाभ्यास के लिए नितान्त आवश्यक हैं और जिनके बिना ध्यान का अभ्यास असम्भव है। कुछ ऐसे आध्यात्मिक गुण हैं, जो ध्यान की उच्चतम अवस्था की पृष्ठभूमि के निर्माण में ईंट का काम करते हैं। ध्यान तो पिरामिड (स्तूप) की नोक कहा जाता है और नोक या चोटी हवा में उत्पन्न नहीं की जा सकती। वह तो ठोस धरती पर बनी प्रशस्त नींव पर ही निर्मित होती है। ध्यान की संरचना विनिर्मित होती जाती है और अन्ततः वह सबसे ऊँचे उस एक पाषाण-खण्ड तक आती है जिसे ध्यान कहते हैं। अतः यह वह प्रक्रिया है जो सद्गुणों पर आधारित है।
सद्गुण आध्यात्मिक गुणों को कहते हैं। आध्यात्मिक गुणों पर इतना आग्रह क्यों है, यह समझना बड़ा सरल है। ये गुण आपके स्वभाव में से उन शक्तियों को निकाल फेंकेंगे जो ब्रह्मानुभूति और आत्मानुभूति के पथ में बाधक और उसकी विरोधी हैं। आपके स्वभाव में जब तक वह बुराई है, आध्यात्मिक अनुभव होना कठिन है। आप यदि चाहें कि आप भीगे और सूखे साथ-साथ रहें, तो यह सम्भव नहीं। अतः उन विकारों को दूर करने का एक ही उपाय है कि आप अन्तर में सबल और निश्चित गतिशीलता उत्पन्न करें, तब वे नहीं रहेंगे। वे रह ही नहीं सकते; क्योंकि वे और कुछ नहीं, विधेयात्मक शक्ति का अभाव मात्र हैं। उनकी निजी सत्ता कुछ भी नहीं है। अतः उन्हें जीतने के लिए आप अपने अन्तर में कुछ विधेयात्मक तत्त्व सृजन कीजिए। इन विधेयात्मक तत्त्वों को ही किसी उत्तम संज्ञा के अभाव में 'सद्गुण' कहा जाता है। आप जिस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उसके प्रत्यक्ष व्याघाती तथा विपरीतधर्मी तत्त्वों को अपनी प्रकृति से बाहर रखने के लिए ये आध्यात्मिक गुण अत्यावश्यक हैं।
उन पर आधारित ध्यान एक आन्तरिक प्रक्रिया है। इन्द्रियों का मुख्य कार्य सदैव आपके मनस्तत्त्व को बहिर्मुखी करके विषयों में उलझाये रखना है। इन्द्रियों का यही स्वभाव है और जब तक आप उनके इस स्वभाव से परिचित हो कर उन्हें वश में नहीं करेंगे, आपका मनस्तत्त्व कदापि अन्तर्मुखी नहीं हो सकेगा। ध्यान के लिए मनस्तत्त्व को समेट कर अन्तर्मुख करना आवश्यक एवं नितान्त अपरिहार्य है। अतः ध्यान के लिए अन्य पूर्व शपथ है इन्द्रिय-संयम। परन्तु यदि अन्तर्मुख होने के उपरान्त भी मनस्तत्त्व निरन्तर स्फुरण की अवस्था में है, तब भी आप ध्यानाभ्यास नहीं कर सकते; क्योंकि ध्यान के लिए कुछ अंशों में निश्चलता की आवश्यकता है। अतः उसके बाद मन को निश्चल करना तथा मन की इच्छाओं को, कामनाओं को, उसकी अनेकानेक महत्त्वाकांक्षाओं को, आसक्तियों को, चाहना को जो उसे निरन्तर उत्तेजना और क्षोभ की अवस्था में रखती हैं-शान्त करना आता है। इन सबको जीतना है और यह एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है। इसमें समय लगता है।
कुछ सीमा तक मन को नितान्त निश्चल बनाने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। वर्ष भी लगते हों, तब भी यह करणीय है। अधैर्य में आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता। उतावली में भी नहीं। उत्साह होना चाहिए, महान् उत्साह, विलक्षण जोश; परन्तु साथ ही धैर्य भी। अतः मन में निश्चलता की अवस्था तब आयेगी जब आप मन में से नाना इच्छाओं को, आसक्तियों को, प्रबल आकांक्षाओं को, अपनी योजना आदि सबको निकाल फेंक देंगे। तभी आपमें एकीकृत एक अभिकांक्षा उदित होगी। मन केवल एक ही चीज चाहता है। अतः उसे और कुछ नहीं चाहना चाहिए। इच्छाओं का पूर्ण अन्त करना असम्भव है। क्षुधा, खाने-पीने की इच्छा, पहनने-ओढ़ने आदि की इच्छाएँ बड़ी बलवती होती हैं। आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। पिता अपने बच्चे के भावी जीवन के लिए योजना बनायेगा; परन्तु उसे एक महत्त्वाकांक्षा के अतिरिक्त अन्य विविध इच्छाओं को नष्ट कर देना होगा।
आकांक्षा केवल एक होनी चाहिए और उसी की पूर्ति हेतु समूची शक्ति लगा देनी चाहिए। आप मन में अपने परम लक्ष्य पर ही अधिक-से-अधिक प्रमुख बल दें। सम्प्रति आप जो जीवन जी रहे हैं, उसकी कुछ अपरिहार्य इच्छाएँ होती हैं जो चाहे मन के इर्द-गिर्द फिरती हों, परन्तु फिर भी मन सापेक्षतः संयुक्त, एकीकृत होता है। यदि वह एकीकृत है, समाहित है तो उसके चतुर्दिक् जो इच्छाएँ हैं, उनका अन्त हो जायेगा। उसमें अन्य कोई इच्छा, आकांक्षा, आसक्ति, कामना, लालसा आदि नहीं रह जायेगी। मन पूर्णरूपेण अन्तर्मुख हो कर एकता की अवस्था में आ जायेगा। इसे हम संस्कृत में एकाग्रता कहते हैं।
एकाग्रता का अर्थ है ध्यान के किसी एक वस्तु पर स्थिर हो जाने की अवस्था। यही मन, जो इन्द्रिय-अनुभवों के परित्याग से, स्थूल विषयों की कामनाओं को सम्पूर्णरूपेण विनष्ट करने से तथा त्याग से अति सूक्ष्म हो गया है, शुद्धता की अवस्था को प्राप्त होता है। देखिए, मन पदार्थ भी है। यह स्थूल पदार्थ की तुलना में अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ है। आत्म-तत्त्व से तुलना करने पर यह पदार्थ ही है। जब यह काम, लोभ आदि सांसारिक वृत्तियों से भर जाता है और रजस् और तमस् की वृत्तियाँ प्रधान हो जाती हैं, तब अशान्ति, स्वार्थपरक इच्छाओं तथा क्रियाओं द्वारा और भी स्थूल हो जाता है और जब वह इन वृत्तियों का अतिक्रमण कर लेता है, उन्हें अपने अधीन कर लेता है, तब वह विशुद्धता एवं सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होता है। ये दोनों ही अवस्थाएँ परस्पर परिवर्तनीय है। सूक्ष्म शुद्धता की अवस्था में मन ऊर्ध्व गति लेता है। परन्तु जब तक मन सूक्ष्म और नितान्त शुद्ध नहीं हो जाता, वह ऊर्ध्व दिशा में आरोहण नहीं कर सकता। उसकी गति सदैव ऊर्ध्व होगी।
मन को इतना शुद्ध और सूक्ष्म बनाने के लिए नितान्त शुचिता, सद्गुण, इन्द्रिय-संयम एवं इच्छाओं और कामनाओं के त्याग की आवश्यकता है, तभी वह आत्म-विचार, सत्य-विचार का साधन बन सकेगा। अन्यथा स्थूल मन आत्म-विचार करने की अवस्था में नहीं होता। आत्म-चिन्तन अथवा आत्म-विचार करने की क्षमता उसमें तभी आती है, जब वह उक्त प्रकार से शुद्ध और सूक्ष्म हो गया हो। उसी मन को ध्यान में लगाना चाहिए। जब तक आपका मन ऐसा नहीं हो जाता, आप ध्यान में नहीं लग सकते। यदि आप सोचते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, तो यह केवल आपका सोचना मात्र है-ध्यान नहीं है। सीधे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं। इन क्षणों में आप मन से कुछ कर अवश्य रहे हैं; परन्तु यह ध्यान नहीं है।
ध्यान के लिए एक दूसरे ही प्रकार का मन चाहिए। बहिर्मुखी मन, विषयाकार मन, कामासक्त मन वास्तव में ध्यान नहीं कर सकता। केवल एकाग्र होने की चेष्टा में कुछ कसरतें कर सकता है और इस अभ्यास के दौरान उसे अनुशासन का मूल्यवान् प्रशिक्षण मिल जाता है। यह प्रशिक्षण बिलकुल व्यर्थ नहीं होता। यह मन को कुछ अंश तक उस दिशा में तैयार करता है; परन्तु आपके अन्तर से पूर्ण परिवर्तन तो मन को नितान्त सूक्ष्मता और शुद्धता की अवस्था में लाने पर ही होता है। ध्यान की अन्तर प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए वैसा मन चाहिए; क्योंकि वही साधन है। सूक्ष्म, शुद्ध, पूर्णरूपेण निश्चल और शान्त तथा सर्वथा अन्तर्मुखी मन ध्यान का साधन है। केवल इसी मन के द्वारा ध्यान किया जा सकता है।
६. भारत : आज और कल
दिव्य हिमालय और पुनीत गंगा-यमुना की इस भूमि की जय हो! हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी को शतशः प्रणाम जिन्होंने हमें भारत, उसके दर्शन, संस्कृति, उसके आदर्श और उसके मूल धर्म का सम्मान करना सिखाया तथा जिन्होंने हमें भारत की ज्ञान-सम्पदा की महानता का ज्ञान कराया, जिनके कारण ही हम इस पुण्यभूमि की पवित्रता और इसके सम्पूर्ण वातावरण की आध्यात्मिकता को जान सके।
कोई भूभाग, देश या राष्ट्र भौगोलिक रूपरेखा और आर्थिक साधनों द्वारा ही नहीं जाना जाता और न वहाँ निवास करने वाली जनता से। युग-युगान्तरों से वहाँ की जनता ने जीवन यापन की जिस पद्धति का क्रमशः विकास किया है, उस जीवन पद्धति से हम किसी राष्ट्र को जान सकते हैं। वही राष्ट्र को बनाती है। वही विकसित जीवन पद्धति है जिसके लिए समूचा देश जीआ और उसने प्रयत्न किया। वर्तमान अतीत की उपज है और भविष्य उसकी (उपज) होगा जो आज हम निर्माण करते हैं। आज और आगामी कल का भारत अनेकानेक शताब्दियों से गुजरती हुई अगणित पीढ़ियों के असंख्य बीते हुए कलों की पूर्ति है।
इस विश्व में मानवता के सम्बन्ध में एक दैवी योजना रहती है। मानव मात्र का सामान्यतः विकास होता है। प्रत्येक राष्ट्र को इस सामान्य विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करना है। अपनी संस्कृति के रूप में अपनी सम्पदा का विश्व-कल्याण तथा विश्व-मानवता की सामूहिक प्रगति के लिए समर्पण भाव ऐसा तत्त्व है जिस पर ईश्वर की योजना क्रियाशील होती है। योगदान की इस भावना को अधिक-से-अधिक महत्त्व देना होगा। मानव-जाति के सामूहिक विकास की प्रगति के प्रति समस्त राष्ट्रों की सामान्य जिम्मेदारी में योग देने की भावना को 'यज्ञ' और 'दान' की भावना कहते हैं। दान का अर्थ है वह वस्तु जो आप दूसरों को स्वेच्छा से देते हैं। मानव-जाति तथा समग्र विश्व की सेवा के अंग के रूप tilde 4 जो उत्सर्ग किया जाता है, वह यज्ञ है।
इस विशाल भारत देश, जो महान् गुरुवरों की पूज्य भूमि, कबीर की, राम की, स्वामी रामकृष्ण की, स्वामी विवेकानन्द की भूमि है— में यज्ञ-भाव को अक्षुण्ण रखने के लिए मानवता के उत्कर्ष हेतु समस्त राष्ट्रों के सामान्य उत्तरदायित्व में भाग लेने के लिए यहाँ की जनता को अपनी महान् थाती की, जो उसे पूर्वजों से प्राप्त हुई है, गौरव-गरिमा को बनाये रखना है।
भारत की महान् भूमि का महत्त्व इसलिए नहीं है कि उसने अनेकानेक शताब्दियों से भौतिकवादी जीवन-पद्धति का विकास करने में अपना ध्यान लगाया, प्रत्युत इसलिए है कि वह आध्यात्मिक मूल्यों की-मानव को भगवत्पुत्र के रूप में लेने के आत्यन्तिक मूल्यों की-भावना-प्रधान भूमि है।
भारतवर्ष की भाग्यशाली सन्तान! तुम यहाँ इस पृथ्वीलोक में यात्री की तरह से हो। अतः यहाँ जीवन का ध्येय स्वयं जीवन ही नहीं प्रत्युत उच्चतर ध्येय है। जीवन हमें एक सुअवसर के, स्वर्णिम अवसर के रूप में-उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस परम दिव्य परमेश्वर से अपने सनातन सम्बन्ध को पहचानने के लिए दिया गया है। आप अपनी आन्तर सत्ता की गहराइयों में सर्वदा उस परम दिव्य चेतना से जुड़े हैं जिसे धर्म भगवान्, परमात्मा, गाड या अल्लाह कहते हैं। आप सब उसी महान् दिव्य सत्ता के बच्चे हैं। संसार केवल एक ही होता है। एक ही है। ईश्वर भी एक ही है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। मानवता एक है और मानवता के इस विशाल परिवार में हममें से प्रत्येक को ईश्वर के नाते-जो हमारा कारण है, हमारा मूल है, आधार है और अन्तिम लक्ष्य है-इतर मानवता से अपनी एकता का सम्बन्ध प्रेमपूर्वक स्वीकार करना चाहिए।
हम भगवान् को सम्बोधित करते हैं-"त्वमेव माता च पिता त्वमेव तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है।" क्या इससे ज्ञात नहीं होता कि आप उसके बालक है और इसी कारण तत्त्वतः दिव्य हैं? पिता और माता की तरह भगवान् दिव्य हैं, अविनाशी, नित्य, सम्पूर्ण, सच्चिदानन्द हैं। अतः उसके बालक होने के नाते आप भी अविनाशी दिव्य आत्मा हैं। यही भारत की इस महान् भूमि की संस्कृति का सार है।
भारतीय संस्कृति का सारे भारत की सन्तानों के लिए तथा समस्त मानवता के लिए सन्देश है- "ओ मानव! तुम तत्त्वतः दिव्य हो। तुम यह मरणधर्मा शरीर नहीं हो, न यह अशुद्ध तथा अशान्त मन ही तुम हो। तुम सर्वदा शुद्ध शान्तात्मा हो। शान्ति ही तुम्हारा नाम है। शान्ति तुम्हारा स्वभाव है। तुम यह तुच्छ, सीमित बुद्धि नहीं हो जो कभी शुद्ध तर्क उपस्थित करती है तो कभी भूलें करती रहती है और अव्यवस्था उत्पन करती रहती है। तुम अनन्त, असीम, नित्य पूर्णात्मा हो।" भारत का यह प्रमुख सन्देश है और इसके ज्ञान में ही आपको यहाँ जीवन यापन करना है। आपको यहाँ अपना उच्च स्वभाव, अपनी आध्यात्मिक चेतना व्यक्त करने के लिए जीवन यापन करना है। इस शुचिता को, इस प्रेम को, इस सदाशयता को तथा इस पूर्णता को जो आपमें आपके अपरिवर्तनशील, नित्य स्वभाव के रूप में विद्यमान है व्यक्त करने हेतु आपको जीना है।
अरे मानव! तुम दिव्य हो; परन्तु अपने मूल रूप को भूल बैठे हो। तुम इन्द्रियों के चंगुल में फँस गये हो और अपने को पहचानने में नितान्त भूल कर बैठे हो। तुम उस रूप को अपना मान बैठे हो जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से सर्वथा भिन्न है और जो तुम्हारी सत्ता के सार-तत्त्व को ही नष्ट कर देता है। तुम अपने महिमावान् स्वरूप को भूल गये हो। तत्त्वतः तुम भागवत चेतना-युक्त ज्योति की; शुचिता, आनन्द और ज्ञान की किरण हो; परन्तु अभी तुम अपनी इन्द्रियों के दास बने हुए हो। तुम्हारा समस्त चिन्तन तुम्हारे तुच्छ अहं से उद्भूत है जिसे तुमने अपनी वास्तविक सत्ता मान लिया है; लेकिन वस्तुतः वह तुम नहीं हो। अतः जग जाओ और अपने असली स्वरूप को समझो, अपने दिव्य स्वरूप को पुनः जान लेने का प्रयास करो।
समस्त आनन्द और उल्लास आपमें ही है। आप स्वयं परमानन्द, परम सुख, असीम शान्ति और पूर्णत्व हैं। यही आपका स्वभाव है। आपकी अन्तरात्मा, आपकी वास्तविक सत्ता तत्त्वतः अनिर्वचनीय आनन्द और शान्ति है। आनन्द के इस जीवन्त बोध का अभिज्ञान वस्तुतः कठिन कार्य है। यही जीवन का महान् प्रयोजन है।
अपने स्वभाव में दिव्यता प्रकट करो। आप देह-स्वभाव या मन के स्वभाव को प्रव्यक्त करने के लिए नहीं हैं। आपको तो भागवत-स्वभाव, अध्यात्म-स्वभाव प्रकट करना है। अन्तर की गहराइयों में छिपे इस अध्यात्म-तत्त्व को जाग्रत करने की कला सीखो-इसे खोजो और प्रबुद्ध प्रयास द्वारा इसका विकास करो।
दिव्यता प्राप्त करो और इस दिव्यता को गरिमा सहित प्रकट करो। अपने जीवन को सत्य से, सौन्दर्य से, अच्छाई और पवित्रता से, सेवा-भावना से, मानव-एकता की भावना से अनुप्राणित कीजिए। भगवान् के नाते आप समस्त मानवता का एक अंश हैं। इसे अनुभव कीजिए। बन्धुत्व की भावना रखिए। वे आपके हैं; अतः उनका दुःख-सुख, सफलता-विफलता आप उसी प्रकार अनुभव करें जैसा वे करते हैं।
भगवान् से कामना है कि आप सभी इस परम लक्ष्य को इसी जीवन में प्राप्त करें! भारत के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का परम आदर्श पूर्णता-प्राप्ति है। यही वास्तविक भारत है।
७. श्री गणेश का सन्देश
श्री गणेश को भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में सिद्धि-विनायक, सिद्धि-दाता अर्थात् सभी कार्यों को पूर्ण करवाने वाला, उनमें सफलता देने वाला माना जाता है। हम आज इस विनायक-पूजा के पवित्र पर्व पर श्री गणेश को अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। हमारे यहाँ हर कार्य या त्योहार के आरम्भ करने से पूर्व श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। लोग गणेश भगवान् के विषय में प्रचलित कथाओं से भली-भाँति परिचित हैं। हम यहाँ यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस देवता के विषय में कोई ऐसी विशेष ज्ञातव्य बात है कि जिसके अध्ययन से हम कुछ विशेष लाभ प्राप्त कर सकें और अपेक्षाकृत अधिक उपकृत हो सकें।
श्री गणेश जी का परम्परागत रूप बड़ा विचित्र है। अनेक व्यक्तियों ने इसके सम्बन्ध में अपनी भिन्न-भिन्न शास्त्रीय व्याख्या देने का प्रयत्न किया है। गणेश जी के स्वरूप की शास्त्रीय व्याख्या से हमारा उतना प्रयोजन नहीं है। हम तो गणेश जी से सम्बन्धित कुछ ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए अत्यन्त शिक्षाप्रद हैं और जिनमें आध्यात्मिक तत्त्व हैं।
हमें सर्वप्रथम जानना चाहिए कि गणेश जी ने हमारे लिए जो एक महान् कार्य किया है, उसके कारण हम जीवन-पर्यन्त उनके सदा ऋणी रहेंगे। वह कार्य अधिकांशतः भुला दिया जाता है और वह कार्य इस प्रकार है। भारत के महान् धर्मग्रन्थ महाभारत की महर्षि वेदव्यास ने समस्त मानव जाति को नीति, सदाचार और धर्म का जीवन व्यतीत कराने वाले धर्म का ज्ञान देने हेतु रचना की थी। महाभारत में उन्होंने वह सभी कुछ प्रस्तुत किया है जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार यह ग्रन्थ एक महान् ज्ञानकोश है, विशेषकर इसका शान्तिपर्व तो ज्ञान की खान है।
कहा जाता है कि विश्व के महान् धर्मग्रन्थों में जो कुछ भी जानने योग्य है, वह सब महाभारत में निहित है और जो महाभारत में नहीं है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है। श्री गणेश जी की ही कृपा है कि आज हमें यह ग्रन्थ उपलब्ध है। महर्षि वेदव्यास के प्रेरक क्षणों में उनकी वाणी से निकला कथन लिखने में कोई भी समर्थ नहीं था। गणेश ही थे जिन्होंने बैठ कर श्री वेदव्यास के श्रीमुख से निःसृत वाङ्मय को लिपिबद्ध किया। यद्यपि महाभारत के प्रणेता श्री वेदव्यास जी हैं; परन्तु वास्तविक लेखक गणेश जी ही हैं जिन्होंने हम मानवों को धार्मिक ज्ञान-सम्पदा दे कर कृतार्थ करने के उद्देश्य से हमारे ऊपर स्नेह-दृष्टि रखते हुए यह श्रमसाध्य कार्य सम्पन्न किया।
इस प्रकार उन्हें भारत के धर्म-तत्त्व का मूल उद्गम मानते हुए हम उनके जीवन की उन दो अद्भुत घटनाओं का उल्लेख करेंगे जो हमारे समक्ष ब्रह्मविद्या के मूल सत्त्व को प्रकाशित करती हैं। कहा जाता है कि गणेश जी के पास अन्य आभूषणों के साथ ही मणिजटित एक अमूल्य हार भी था। इस हार की कथा की पृष्ठभूमि भी इस प्रकार है। एक दिवस भगवान् शिव माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के संग बैठे हुए थे। माँ पार्वती के मन में अपने दोनों पुत्रों की पृथक् पृथक् शक्ति और ज्ञान-क्षमता जाँचने की इच्छा उदित हुई। अतः उस समय वे जो हार पहने हुई थीं, उसे उतारा और बोलीं- "देखो, यह हार है। तुम दोनों में से जो भी अखिल ब्रह्माण्ड की एक बार परिक्रमा करके मेरे पास पहले पहुँचेगा, उसे मैं यह हार दूँगी।"
भगवान् कार्तिकेय ने सोच लिया कि यह तो मुझे ही मिलेगा। गणेश इस भारी- भरकम शरीर से ब्रह्माण्ड की परिक्रमा कैसे कर सकेंगे? उनके लिए यह अति-कठिन होगा। कार्तिकेय का वाहन मोर भी अति तीव्र गति वाला था और उन्हें तुरन्त ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करवा सकता था। अतः वे तत्काल ही मोर पर सवार हो कर निकल पड़े। लेकिन विनायक किंचित् भी परेशान नहीं हुए; बड़ी देर तक अपने माता-पिता के पास बैठे रहे। जब उन्हें लगा कि कार्तिकेय के पहुँचने का समय निकट आ गया है, वे उठे और शिव-पार्वती के चारों ओर प्रदक्षिणा करके माँ को साष्टांग प्रणाम किया और उनके सम्मुख हाथ फैला दिया।
देवी पार्वती उनके इस कार्य में छिपे ज्ञान की गहराई को समझ गयीं। उन्होंने देखा कि गणेश की सहज प्रज्ञा कुछ इस प्रकार की है कि उन्हें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही शिव-शक्ति से विनिर्मित दिखायी दिया। उन्हें दिखायी पड़ा कि सम्पूर्ण विश्व में वे (शिव-शक्ति) परिव्याप्त हैं और सारा विश्व उनमें है। इस प्रकार उन्हें हार की प्राप्ति हुई। अत्यन्त परिश्रम के उपरान्त परिक्रमा करके जब कार्तिकेय लौटे, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश को पहले ही पुरस्कार मिल चुका है।
यह एक छोटी-सी लघु-कथा है; परन्तु इसमें उपनिषदों का उच्चतम ज्ञान निहित है। अर्थात् 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' - जो-कुछ है, सब वही सर्वशक्तिमान् है। इसी सर्वशक्तिमान् ने स्वयं को समग्र विश्व-रूप में प्रक्षेपण किया है; अतः हम उस सर्वशक्तिमान् का सम्मान करते हैं और साथ ही अखिल ब्रह्माण्ड का भी।
गणेश जी अखण्ड ब्रह्मचारी हैं। उनकी कोई सहधर्मिणी नहीं है। उनके इस ब्रह्मचर्य व्रत के सम्बन्ध में भी एक कथा है जिसका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण आशय है। कहा जाता है कि गणेश जी जब छोटे थे, उन्होंने खेल-खेल में एक बिल्ली को पीटा और पीट-पीट कर आहत कर दिया। इसका क्या परिणाम होगा, वह नहीं जानते थे। खेल समाप्त होने के कुछ देर बाद जब वे अपनी माता देवी पार्वती के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि माँ पार्वती के शरीर पर गहरी चोटों के निशान पड़े हुए हैं। बालक गणेश यह देख कर घबरा गये और पूछने लगे कि यह क्या हुआ, किसने उन पर प्रहार करके ऐसा घायल कर दिया? जननी पार्वती बोलीं- "और कौन कर सकता है? यह तो तुम्हारे अपने हाथों से हुआ है।"
क्षण-भर गणेश जी की समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे सम्भव हुआ? अतः वे माता पार्वती से बोले-"तुम्हारा क्या आशय है माँ? मैंने तो तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचायी?" तब माँ ने कहा- 'वत्स! याद करो, दिन-भर में तुमने आज किसी जीव को चोट पहुँचायी है या नहीं?" गणेश जी ने पल-भर सोचा और उन्हें तत्क्षण बिल्ली के संग किया हुआ खिलवाड़ याद आ गया। "हाँ, माँ, एक बिल्ली को मैंने पीटा था, और तो कुछ नहीं किया।" माँ पार्वती ने मुस्कराते हुए कहा- "क्या तुम नहीं समझते कि संसार में जितने भी नाम-रूप हैं, वह मैं ही हूँ? मैं ही वह सब नाम-रूप बन गयी हूँ। इस विश्व में मेरे सिवा कोई नहीं है। विश्व में सिवाय तुम्हारी माँ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।"
देवी पार्वती ने जब यह प्रकट किया, तब यह सत्य उस देव बालक की अन्तश्चेतना में बैठ गया और उन्होंने प्रण किया कि वे जीवन-पर्यन्त विवाह नहीं करेंगे; क्योंकि जब उन्हें ज्ञान हो गया कि समस्त विश्व में जो नाम-रूप हैं, उनमें उनकी माता ही प्रव्यक्त हैं तो समस्त स्त्री-जाति उनकी माता सदृश हो गयी। श्री गणेश जी के ब्रह्मचर्य की इस कथा में एक विशेष अर्थ निहित है। यह हमारे समक्ष वेद और उपनिषदों, आगम और शास्त्रों के गुह्यतम ज्ञान का उद्घाटन करती है। यथा इस कथा द्वारा हमें बताया जाता है- 'सर्वं शक्तिमयं जगत्' - इस विश्व में जो-कुछ भी है, वह सब सर्वशक्तिमान् प्रभु की शक्ति का ही व्यक्त रूप है।
श्री गणेश जी के जीवन की ये दो घटनाएँ ब्रह्मविद्या का सार हैं और उपनिषद् की प्रमुख उद्घोषणाएँ हैं- 'सर्व ब्रह्ममयं, सर्वं शक्तिमयम्।' दृश्य जगत् और परम सत्ता में अनन्य एकता तथा सृष्टि के समस्त नाम और रूपों में परम सत्ता की परिव्याप्ति, ये दो महान् सत्य बड़े सशक्त रूप में हमारे और साधकों के लिए उद्घाटित हुए हैं।
हम भगवान् गणेश जी की उपासना करते और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी उसी प्रकार का आत्मबोध करायें जैसा उन्हें माता पार्वती से हुआ। अतः इस महा सिद्धि-विनायक से हम प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर भी जगज्जननी देवी पार्वती कृपा करें और जैसे उन पर परम सत्य प्रकट हुआ है, हमारे समक्ष भी हो जिससे हमें बोध हो सके कि जो कुछ है, वह परमेश्वर ही है और वह परमेश्वर ही यह सम्पूर्ण जगत्- नाम-रूप बन गया है।
गणेश जी का आकार भी साधकों को कुछ महत्त्वपूर्ण संकेत देता है। एक तो सर्प है जो उन्होंने कटि में बाँधा हुआ है। कहा जाता है कि सर्प अहंकार का चिह्न है। अतः उनका यह अद्भुत आभूषण अहंकार पर उनके पूर्ण नियन्त्रण का संकेत देता है।
एक घटना और भी है कि वे चन्द्रमा पर क्क्रुद्ध हो गये और उस पर अपना दाँत फेंक कर उसके अभिमान को पराजित किया। इससे योग की प्रक्रिया का ज्ञान होता है अर्थात् मन की समस्त क्रियाओं को शून्य कर देना अथवा मन को क्रिया-रहित कर देना। चन्द्रमा मन का अधिष्ठातृ देवता है। विराट् पुरुष के चित्त से निकली हुई यह एक विशेष शक्ति है और चन्द्रमा को पूर्णतः अधीन कर लेना मनोनाश अथवा मनोलय का सूचक है।
इस प्रकार अहं-चेतना जो पार्थक्य लाती है, उसका विनाश तथा पूर्ण मनोनाश व्यावहारिक योग-साधना के दो प्रधान रहस्य हैं जो गणेश जी अपने व्यक्तित्व द्वारा प्रकट करते हैं।
८.दिव्य बनो
मोक्ष, शाश्वत जीवन और स्वर्ग के राज्य का आधार, ईश्वर-साक्षात्कार का, समाधि का, आत्मोपलब्धि का, वैश्विक चैतन्य का, निर्वाण आदि सबका आधार है। सदाचार, शुद्ध चरित्र, सद्गुण, शुचिता, सत्य, दयालुता, करुणा, सरल जीवन, आत्म-संयम, विनम्रता, कामना-जय, सबमें समत्व की भावना और व्यर्थ की चर्चा में समय का अपव्यय न करना, गप्प न करना तथा विविध व्यर्थ के विचारों से स्वयं को मुक्त रखना, स्वयं को व्यर्थ की खोज में न लगाना और लौकिक इच्छाओं से दूर रहना-संक्षेप में यह ईश्वरोन्मुख, ईश्वर-केन्द्रित जीवन है, दैवी सम्पदा और दैवी गुणों से सम्पन्न चरित्र के साथ दिव्य जीवन जीना है। शाश्वत आधार यही है। आध्यात्मिक जीवन में इसकी कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते।
जो व्यक्ति शान्ति चाहता है और वास्तविक सुख का अभिलाषी है, उसे भला रहना है और सत्पथ का अनुसरण करना है; क्योंकि सुख सद्-जीवन से, पवित्र जीवन से, धार्मिक जीवन से ही उद्भूत होता है। धार्मिक जीवन कठिन है, प्रीतिकर नहीं है। वह व्यक्ति के लिए बहुत कठोर, कष्टकर तथा अत्यधिक त्रासक होता है; परन्तु अकथनीय, अवर्णनीय और अतुलनीय सुख भी यदि कोई प्रदान करता है, तो यह धार्मिक जीवन ही करता है।
सुख में सब दुःखों को जीतने की शक्ति है। वह सब यातनाओं को, कठिनाइयों को, बाधाओं को जीतने की शक्ति रखता है। बहुधा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भद्र दिखायी देता है, उसे देख कर लगता है कि वह अनेक कठिनाइयाँ झेल रहा है; लेकिन जो व्यक्ति अच्छे गुण वाला नहीं है, वह अति-प्रसन्न दिखायी देता है। यह हमारे अनुभव की बड़ी विचित्र-सी भ्रमपूर्ण स्थिति है। ऊपरी सतह के नीचे क्या है, हम देख नहीं पाते। भला आदमी अधिक कठिनाइयाँ झेल सकता है; परन्तु साथ ही वह सुखी भी अधिक मात्रा में होगा और उसका हृदय शान्ति और आनन्द से पूर्ण होगा। वह दुःख झेलेगा; परन्तु बड़ा सुखी और शान्त रह कर नींद भर सोयेगा। वह भय-रहित होगा।
कुकर्मी, कुमार्गी जो सद्-जीवन व्यतीत नहीं करता, प्रत्यक्षतः आराम का जीवन व्यतीत करता-सा प्रतीत होता है; परन्तु वस्तुतः वह बड़ा उद्विप्न, अशान्त रहेगा-हृदय से उद्विग्न और मन से अशान्त। उसे वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। सुख बहिर्मुखी अवस्थाओं से निरपेक्ष होता है। विपत्तियाँ और कठिनाइयाँ तथा सुख एक-साथ उपस्थित रह सकते हैं। यह बिलकुल निश्चित है। आराम, सुविधाएँ और सुख, दुःख, अशान्ति, आन्तरिक व्यग्रता, असन्तोष और अतृप्ति सह-अस्तित्व रखते हैं।
विश्व-विधान है कि सुख और शान्ति धर्मोदय के साथ आती है। शाश्वत नियम यही है कि आनन्द धर्मात्मा को और शान्ति सदाचारी को उपलब्ध होती है। जो धर्मात्मा है, उसे सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है।
धर्म का पथ ही परम सौभाग्य का, परम आनन्द और परम शान्ति का पथ है। यही सत्य है और परमानन्द, ब्रह्म-साक्षात्कार का आधार है। जीवन में अच्छाई और सत्य के पथ का अनुसरण करने से दिव्यानन्द और नित्य शान्ति प्राप्त होती है। जो दिव्य जीवन हमारी आन्तरिक आध्यात्मिक शक्तियों को विकास देता है, वह निःस्वार्थता का, सेवा, भक्ति और उपासना का जीवन है, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का जीवन है। यह अविरत इस जिज्ञासा से पूर्ण है कि मैं कौन हूँ, और मैं क्या हूँ और यह दृढ़ निश्चय करने के लिए है कि मैं यह शरीर, यह मन और यह बुद्धि नहीं हूँ प्रत्युत अन्तरात्मा, परम आत्मा, नाम-रूप-हीन, अजन्मा, अविनाशी, अमर, अक्षर, नित्य आत्मा हूँ। मैं सोऽहं, हंसः सच्चिदानन्द हूँ।
अतः सत्यता, शुद्धता, सरलता, विनम्रता, सदाचरण, दृढ़ चरित्र एवं आत्म- संयम निष्कामता पर आधारित जीवन-आध्यात्मिक जीवन यापन करो। सम्पूर्ण कार्यों और कर्तव्यों को सद्भावना से पूर्ण करते हुए, उनके बीच भी ईश्वर को परम लक्ष्य मानना, इस महान् लक्ष्य को सदैव याद रखना, नित्य प्रेम और श्रद्धापूर्वक ईश्वर को स्मरण करना, उन्हीं को सबमें देखना, पूजा-भाव से समस्त कार्य करना, निःस्वार्थता, सेवा, भक्ति, पूजा एवं धारणा, ध्यान तथा सतत आत्म-जिज्ञासा द्वारा उन्नति करते हुए ब्रह्मज्ञान प्राप्त करो; दिव्यानुभव, आत्मानुभव, आत्म-साक्षात्कार की महान् अवस्था प्राप्त करो।
इस अवस्था को सच्चिदानन्द प्राप्त कर आपको अनुभव और बोध हो जायेगा कि 'मैं परम हूँ, आत्मा हूँ, अजर, अमर हूँ, शान्तात्मा हूँ, अभय हूँ, विशोक हूँ। अविनाशी हूँ, आनन्द हूँ, शान्ति हूँ। चाहे मैं युवा हूँ, वृद्ध हूँ, स्त्री अथवा पुरुष हूँ, बलहीन या बलवान् हूँ, निर्धन या धनी हूँ, हर स्थिति में मैं वही हूँ। यह शरीर किसी भी अवस्था में, स्थिति में हो, मन भी सुखी या दुःखी हो, इसका कोई महत्त्व नहीं है। मैं न दुःखी हूँ, न सुखी; क्योंकि मैं नित्य वही हूँ, हर स्थिति में सच्चिदानन्द हूँ। देह चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सुविधाजनक अथवा सुविधाहीन-किसी भी स्थिति में हो, मन भी चाहे तुष्ट हो या असन्तुष्ट, विशाल हो या संकीर्ण-मैं हर दशा में, हर देश-काल में, सभी परिस्थितियों में परम सत्य हूँ। चाहे मैं चिथड़े पहने हूँ, बेकार हूँ, बीमारी से ग्रस्त हूँ। चाहे समाज ने मुझे ठुकरा दिया हो, चाहे मेरे परिवार ने मेरा बहिष्कार कर दिया हो, चाहे मैं मित्र-हीन हूँ और मेरी देख-रेख करने वाला भी कोई न हो, तब भी मैं सत्-चित्-आनन्द-सच्चिदानन्द हूँ। ये बाहरी परिस्थितियाँ मेरे वास्तविक स्वरूप को, मेरी मूल सत्ता को, देदीप्यमान् सत्ता को स्पर्श या मलिन नहीं कर सकतीं।'
वह अनुभव जो और सब वस्तुओं का अतिक्रमण कर जाता है, परम और आत्यन्तिक है। इस महा-अनुभव के होने पर व्यक्ति आनन्द से भर उठता है, 'आनन्दोऽहं, आनन्दोऽहं, ब्रह्मानन्दोऽहम्' कहने लगता है। इसे उपलब्ध करके व्यक्ति समस्त परिस्थितियों, अवस्थाओं तथा समस्त द्वन्द्वों को जीत लेता है और सर्वोपरि हो जाता है।
लेकिन वह आश्चर्यजनक अनुभव है क्या? श्री गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज को एक गीत बहुत पसन्द था। उसे वे 'डिवाइन इंजेक्शन' कहा करते थे। 'डिवाइन इंजेक्शन' नामक गीत का एक बार भी उच्चारण आपको इस भौतिक स्तर से ऊपर उठा कर आपके वास्तविक स्वरूप की दिव्य चेतना में ले जाने में समर्थ है। यह आपको अपने जन्म-सिद्ध अधिकार का स्मरण दिलाता है और उस अधिकार को अभी इसी जीवन में अधिगत करने की आपमें प्रेरणा भरता है। 'डिवाइन इंजेक्शन' आपके असली स्वरूप का गीत है। लोग इसे 'चिदानन्द-गीत' भी कहा करते थे और मुख्य अवसरों पर गुरुदेव जब कभी भी श्रोताओं के बीच में होते, वे गुरुदेव से इसे सुनाने का आग्रह करते। सन् १९५० की अपनी अखिल भारतीय यात्रा में उन्होंने इसे पूरे भारत में गाया था।
'चिदानन्द-गीत' आपमें से भी बहुत से जानते हैं। चिदानन्द मेरा नाम नहीं है, यह आपका असली नाम है। मेरा भी असली नाम है। आप इसे अनुभव कर सकेंगे और अनुभव करके कह उठेंगे-"मैं चित् हूँ, आनन्द हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, निश्चिन्त और निर्भीक हूँ, मुक्त हूँ, नित्य पूर्ण हूँ, मैं चिदानन्द हूँ।" यह मत सोचिए कि आप इस अनुभव तक पहुँच चुके हैं। सदैव ध्यान में रखिए कि लक्ष्य एकमात्र यही है और यही बीज रूप में विद्यमान है। वह गुप्त और सुप्त अवस्था में आपमें वर्तमान है। अतः जागिए, उठिए और उठ कर इस महान् अनुभव की ओर बढ़िए। अन्तर के सुमन को मुकुलित करने के लिए जो-कुछ आवश्यक है, वह सब कीजिए। आपको इसके लिए श्रम करना होगा।
यह उपलब्धि आपमें पहले से ही है। आपके भीतर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई अमूल्य और अनुपम सुन्दर हीरा किसी बक्स में बन्द हो और बक्स की कुंजी न मिल रही हो। हीरा प्राप्त करने के लिए आपको बक्स खोलना पड़ेगा। इसी प्रकार यह 'नित्य पूर्णत्व' आपमें सुप्तावस्था में विद्यमान है। आप पहले से ही वह 'पूर्ण' है। बिलकुल जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं-इस अवस्था में आप सत्-चित्-आनन्द हैं-पूर्ण आत्मा हैं। आप सच्चिदानन्द चेतना हैं। यही आपकी वास्तविक चेतना है। जिस चेतना में आप अनुभव करते हैं- 'मेरा घुटना दुख रहा है, मैं इतनी देर बैठा रहा, मेरी कमर में पीड़ा होने लगी' आदि-आदि, वह देह-चेतना या भौतिक चेतना है।
हमें तो कठिनाइयों का सामना करना है। हम न तो उनकी गति में कुछ उलट-फेर कर सकते हैं और न उन समस्याओं की उपेक्षा ही कर सकते हैं जिन्हें सुलझाना है। अतः साधना अपरिहार्य है। आत्म-साक्षात्कार साधना द्वारा होता है। साधना क्या है? साधना का अर्थ है सम्यक् जीवन यापन, भागवत जीवन जीना जिसमें आप अपने वास्तविक स्वरूप को, जो आप वास्तव में हैं उस स्वरूप को, जो सर्वथा शुद्ध और निर्मल है, अभिव्यक्त और अविभव्यंजित करना आरम्भ कर दें। अतः आप इस नित्य-शुद्ध, निर्मल स्वभाव को अपने विचारों में, वाणी में, इच्छाओं में तथा दैनिक जीवन के आन्तरिक उद्देश्यों में व्यक्त करें। इसका अभ्यास कीजिए, इसे जीयें, इसकी किरणों को फैलायें, यही साधना है। आप परम सत्य हैं। इस सत्य को अभिव्यक्त करें। मिथ्यात्व को अपने हृदय से समूल निकाल फॅकिए और साक्षात् सत्यस्वरूप हो जाइए, जो आप हैं वही हो जायें। अपने जीवन को, जो आप वास्तव में हैं, उसके प्रतिकूल न बनायें। तत्त्वतः यही साधना है। मनसा वाचा-कर्मणा दिव्य हो जाना ही दिव्य जीवन यापन का प्रत्यक्ष मार्ग है।
महात्मा गान्धी सत्य को ईश्वर समझते थे। सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। वे भारतीय इतिहास के एक महान् पुरुष थे, महान् नेता थे। उन्होंने सत्य के रूप में सत्य के द्वारा ईश्वर के दर्शन किये थे। यह साधना है। आप भी इसे पा सकते हैं। भागवत जीवन द्वारा, दिव्य जीवन द्वारा इस महान् उपलब्धि को प्राप्त हो जाइए। जो-कुछ आप करते हैं, उस अपनी करनी में और अपनी अन्तरतम निगूढ़ विचारणा में आध्यात्मिक हो कर जीवन यापन करें। एक-एक पग, एक-एक ईंट से साधना का महान् भवन रचा जाता है। आध्यात्मिक प्रयत्न आनन्द है। महान् उपलब्धि हेतु जीवन यापन स्वयं अपने में महिमामय है।
दिव्यता की अभिव्यक्ति से अधिक आप किसे महत्त्वपूर्ण समझते हैं? आप अपने जीवन को अपने वास्तविक स्वभाव के नितान्त प्रतिकूल न बनाइए। यदि आप सदैव अपने सत्स्वरूप के प्रतिकूल चलते रहेंगे, तो आपकी रक्षा कौन कर सकता है? कौन आपको मुक्ति दे सकता है? आप अपने कर्म और अपने इस जीवन के कारण अपने मार्ग में स्वयं ही रुकावट बन रहे हैं और दिव्य जीवन के विपरीत जीवन यापन द्वारा अपना वास्तविक सुख, आनन्द और शान्ति नष्ट कर रहे हैं।
जीवन को भागवत जीवन बना कर और अपने प्रत्येक कर्म को, विचार को, वाणी को भागवत गुणों से ओत-प्रोत करके जीवन यापन करना ही साधना है। दिव्य जीवन यापन करते हुए, अपने जीवन में सर्वत्र अन्तर की दिव्यता को अभिव्यक्ति देते हुए इस दिव्यानुभूति को प्राप्त कर आनन्दित रहो। बड़े प्रसन्न मन से कहो- " चिदानन्द हूँ, ॐ, मैं हर स्थिति में चिदानन्द हूँ।" इसी के लिए प्रयास करो और अपने जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। इसकी उपलब्धि के लिए चाहे कितना ही परिश्रम हो, थोड़ा ही कहा जायेगा। प्रसन्नता और आशा के साथ धैर्यपूर्वक इस लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। कार्य करते समय भी इसका ध्यान रखो, स्मरण रखो। प्रत्येक वस्तु में हर क्षण उसे ही पाने का यत्न करो। परिस्थितियों पर विजय पाओ। मन के विजेता, इन्द्रियजित तथा अपने भाग्य के विधाता बनो।
मैं पुनः कहता हूँ कि आप इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यत्न करें। पर्वत के शिखर तक पहुँचना चाहते हो, तो पर्वत पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा और जिस समय आप सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाओगे, समस्त किया हुआ श्रम आपको बच्चों के खेल जैसा लगने लगेगा। परन्तु तब तक, वहाँ पहुँचने तक आपको निरन्तर क्रमिक रूप से एक-एक पग आगे बढ़ने का श्रम करना पड़ेगा। आप स्वयं में यह भावना और बोध रखिए कि आप पहले से ही शिखर पर हैं; परन्तु चढ़ते जाइए, रुकिए मत। साधना का यही रहस्य है।
ईश्वर आप पर कृपा करे! उसकी असीम कृपा की आप पर अनन्त वर्षा हो ! श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का यह आशीर्वाद सदा आजीवन आपके साथ रहे, आपको सफलतापूर्वक दिव्य जीवन यापन के योग्य बनाये तथा सद्गुणों से आपके जीवन को दीप्त बनाये! आपके सच्चरित्र का विकास हो! आप सत्पथ पर, पुनीत पथ पर चलें। सत्य, पवित्रता और अच्छाई के पथ पर और उस महान् लक्ष्य के प्रति अग्रसर हों जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे आप इसी शरीर से पाने के और अनुभव करने के अधिकारी हैं। अपने इस कार्य को स्थगित न कीजिए। उठिए और इसमें लग जाइए। इस सेवक की प्रार्थनाएँ सदैव आपके साथ हैं। आप विजयी हों तथा इसी जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करें! ईश्वर-चेतना की, ईश्वर-ज्ञान की महिमा से आप भरपूर रहें!
९. देवी-माहात्म्य
पुराण वे शास्त्र हैं जिनके माध्यम से प्राचीन कालीन ऋषियों ने हमारे लिए ज्ञान, प्रेरणा और निदेशों का अमूल्य आगार प्रस्तुत किया है। इन ग्रन्थों में महर्षियों ने मानव-जीवन के गम्भीर तथ्य तथा इस जीवन तथा पारलौकिक जीवन की सफलता का रहस्य गुम्फित कर दिया है। अतः पुराण अध्यात्म-विद्या के आगार हैं, जीवन की विशाल तात्त्विक ज्ञान-सम्पदा के ऐसे कोश हैं जिन्होंने भारत की विश्रुत सभ्यता और संस्कृति की प्रगति और विकास में अत्यधिक सहायता पहुँचायी है। पुराण वह साँचे हैं जिनमें मानव की निम्न प्रवृत्ति को जीतने, पूर्णता-प्राप्ति और उन्नत ईश्वरीय चेतना के महान् लक्ष्य तक पहुँचने की विधियों और साधनों का ज्ञान ढाला गया है। उन्होंने कथ्य को बोधप्रद कथाओं, गहरे रहस्यमय संकेतात्मक विवरणों और रूपकों द्वारा समझाया है।
वे ऋषि जानते थे कि हिन्दू मूलतः स्वभाव से धार्मिक और अन्तर से आस्थावान् हैं; अतः उन्होंने अपने रूपकों और रूपात्मक विवरणों का ताना-बाना ईश्वर के किसी सशक्त और स्थायी रूप अथवा किसी महा-विश्रुत ऋषि के चारों ओर बुना है। प्रायः प्रत्येक पुराण में इस प्रकार का कोई-न-कोई देव या देवी ही उस पुराण का मुख्य पात्र होता है। इसीलिए शिवपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराण, वाराहपुराण, मत्स्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण, नारदपुराण आदि हैं। मार्कण्डेयपुराण के एक महत्त्वपूर्ण अध्याय में देवी-माहात्म्य का सुप्रसिद्ध अंश है जिसमें ईश्वर के देवी या शक्ति रूप की महिमा का वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ में सात सौ श्लोक हैं, अतः इसे देवी सप्तशती भी कहते हैं। देवी-माहात्म्य का कथा-सार संक्षेप में इस प्रकार है।
सुरथ नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। शत्रुओं से पराजित होने पर वह राजधानी से भाग कर जंगलों में भटकता फिरने लगा। यहाँ उसकी भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई। दोनों की परिस्थिति समान ही थी। वह सब-कुछ खो कर निर्धन हो गया था; अतः उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उसका परित्याग कर दिया था। राजा और वैश्य दोनों ही उदास थे; परन्तु दोनों ही मोहवश निरन्तर अपने परिवार तथा धन-सम्पत्ति के सम्बन्ध में सोचते रहते थे। वे आपस में बात करने लगे, उन्हें आश्चर्य था कि जिन लोगों से, वस्तुओं और स्थानों से उन्हें इतना दुःख और कष्ट प्राप्त हुआ था, उनका चित्त पुनः-पुनः उन्हीं लोगों में, वस्तुओं और स्थानों में जा कर क्यों केन्द्रित होता है?
इस परेशान करने वाली समस्या के निदान हेतु वे दोनों एक मुनि के निकट गये जो उसी वन में रहते थे। उनके प्रश्न के उत्तर में मुनि ने बताया कि देवी-शक्ति महामाया की रहस्यमयी शक्ति के कारण ही उनका मन इस प्रकार व्यवहार कर रहा है। राजा सुरथ और व्यापारी समाधि यह सुन कर देवी-शक्ति महामाया के तथा उसकी लीला और महिमा के सम्बन्ध में और अधिक जानने को उत्सुक हो उठे और तब मुनि ने देवी-माहात्म्य का वर्णन किया जो इस प्रकार है:
सृष्टि से पूर्व कल्प के आरम्भ में जब भगवान् महाविष्णु क्षीरसागर (एकार्णव) के विशाल वक्ष पर शयन कर रहे थे, उनके विश्व-रूप से दो महाभयानक असुर मधु और कैटभ प्रकट हुए। वे बड़े भयंकर थे, बड़े हिंसक थे। अतः ब्रह्मा को देखते ही वे उनका संहार करने को दौड़ पड़े। उन बलशाली असुरों की प्रताड़ना और कुभावनाओं से तंग आ कर भयभीत हो ब्रह्मा ने परम अनिर्वचनीय देवी-शक्ति-आदिशक्ति-पराशक्ति का आह्वान करके उसकी कृपापूर्ण सहायता की याचना की।
माँ शक्ति प्रकट होती हैं और भगवान् नारायण को महानिद्रा से जगाती हैं। भगवान् मधु और कैटभ से युद्ध करते हैं और युद्ध में दोनों का संहार कर डालते हैं। यहाँ देवी-माहात्म्य के विवरण का प्रथम अंश समाप्त हो जाता है।
माँ शक्ति की विजय पर समस्त देव गण जय-जयकार करने लगे। महिषासुर नामक एक महाबली असुर ने देवताओं पर विजय पा कर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। उससे तीनों लोक थरथराते थे। माँ शक्ति की विजय पर देवों की जय-जयकार का कोलाहल सुन कर वह क्रुद्ध हो उठा। अब तक वह स्वयं को ही सर्वोपरि समझता था। वह अत्यन्त गर्व से भरा था। कोई उसके बल को चुनौती दे, यह उसे असह्य था; अतः उसने देवी-शक्ति से, जिनकी देव गण जय-जयकार कर रहे थे, युद्ध करने की ठान ली और हाथ में शस्त्र लिये उनके समक्ष आ पहुँचा। भयानक युद्ध हुआ: महाभयंकर संग्राम। असुर सभी ओर से लड़ रहा था, भयानक रूप धारण कर-करके लड़ रहा था; परन्तु प्रकाश के समक्ष अन्धकार टिक नहीं सकता। दिव्य शक्ति पराशक्ति है। सत्य सदा विजयी होता है। परम सत्य की विजय होती है। देवी असुर का संहार कर देती है और इस प्रकार दानवता पर दिव्यता की विजय होती है। इस प्रकार देवी-माहात्म्य का दूसरा अंश समाप्त होता है।
देवी माँ, जिसकी महिमा त्रिलोक में प्रकाशित है, वही शैल-पुत्री के रूप में हिमालय प्रदेश में अवस्थित थीं। उन दिनों शुम्भ और निशुम्भ नामक शक्तिशाली असुरों ने समस्त लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उन्होंने समस्त देवों, यक्षों, गन्धर्वो, किन्नरों आदि को अपने अधीन कर लिया था और उनकी सर्वोत्तम वस्तुओं जैसे ऐरावत, उच्चैःश्रवा, कामधेनु, कल्पवृक्ष आदि पर अपना अधिकार कर लिया था। वे अपने बल और विजय के मद में चूर हो रहे थे। उनकी इच्छा तृप्त होने वाली नहीं थी। वे अधिक-से-अधिक ले लेना चाहते थे।
इन असुरों के दरबार के दो दूतों ने देवी को देखा, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें उनके स्वामियों की सम्पत्ति होना चाहिए। अतः उन्होंने अपनी इस खोज की खबर शुम्भ को दे दी। शुम्भ ने तुरन्त ही देवी को लेने के लिए अपने एक राजदूत को उनके पास भेजा। देवी ने कहा- "मैं उसी के पास जाऊँगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा।" और दूत के संग जाना उन्होंने अस्वीकार कर दिया। दूत ने जा कर यह समाचार शुम्भ को दिया। वह आग-बबूला हो उठा। उसने धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन देवी-शक्ति पर हाथ धरना चाहता था कि देवी ने क्रोधपूर्ण एक हुँकार मात्र से उसे जला कर भस्म कर दिया। वह देवी के क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया।
तदुपरान्त रक्तबीज युद्ध के लिए आता है। वह ऐन्द्रजालिक शक्तियों से सम्पन्न था और साथ ही उसे वरदान भी प्राप्त था जिससे जब कभी भी उसके शरीर के रक्त की एक बूँद पृथ्वी पर गिरती थी, तो उससे एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था। अतः जितनी बार देवी ने उसे घायल किया, उसके रक्त से अगणित शक्तिशाली असुर उत्पन्न हो-हो कर युद्ध-क्षेत्र को भरने लगे। इस पर देवी ने काली का आह्वान किया। सर्वशक्तिमयी काली रक्तबीज का संहार कर उसके घावों से प्रवाहित रक्त को अपनी भयानक लपलपाती जिह्वा से चाटती गयीं कि कहीं उसका रक्त भूमि पर न टपक जाये। इस प्रकार देवी के द्वारा रक्तबीज का विनाश हुआ।
अब शुम्भ और निशुम्भ ने आ कर देवी का सामना किया। महायुद्ध आरम्भ हुआ। निशुम्भ मारा गया। अन्त में शुम्भ को भी देवी ने अपने त्रिशूल से मार गिराया। इस प्रकार दानवी शक्तियों का विनाश हुआ। दैवी विधान विजयी हुआ। अविद्या पर विद्या की विजय हुई। प्रकाश ने अन्धकार को जीत लिया। अज्ञान के विनाश से ज्ञान का प्रकाश हुआ। सर्वत्र आनन्द, उल्लास और अमरता का राज्य हुआ। माँ देवी जी अपनी परम महिमान्वित विजयश्री सहित विराजती हैं। महाशक्ति की जय हो! माँ की जय हो!
१०. साधन-विघ्न : उन पर विजय
अपने हृदय-उपवन में दिव्य गुणों के पुष्प उगाओ। दिव्य गुणों से ही व्यक्ति पवित्रता और पवित्रता से दिव्यता और दिव्यता से ईश्वर-साक्षात्कार तक उठता है। व्यक्ति अशुद्धता से शुद्धता, शुद्धता से शुचिता और शुचिता से उदात्त आध्यात्मिक अनुभव की ओर अग्रसर होता है।
आदि शंकराचार्य जिन्होंने भारत में केवलाद्वैत की स्थापना की, उनके विचार में आत्मा जब ब्रह्मानुभूति हेतु आरोहण करती है, तब उसके इस व्यावहारिक साधना-मार्ग में तीन मुख्य बाधाएँ उपस्थित होती हैं जिनका अतिक्रमण करना होता है। हमारी चेतना चूँकि हमारे रूप से और हमारी देह से बँधी है; अतः हम चेतना की स्थूल अवस्था में हैं। देहगत अवस्था के कारण स्थूल अवस्था हो जाती है; क्योंकि एक अनिर्वचनीय गूढ़ तत्त्व के कारण 'हम' जो इस देह में निवास करते हैं, मानसिक रूप से देह से पूर्ण तादात्म्य कर लेते हैं और इस तादात्म्यता के कारण, देहाध्यास के कारण समझने लगते हैं कि 'हम' यह शरीर हैं और यह शरीर ही 'हम' हैं।
मुख से चाहे आप कितना ही कहते रहें कि 'मैं यह शरीर नहीं हूँ; परन्तु दूसरे ही क्षण अपने जीवन और व्यवहार में प्रकट कर देते हैं कि 'मैं शरीर हूँ'। अतः व्यवहार में हम देह-चेतना को ही व्यक्त करते हैं, कथन में चाहे हम इसके विपरीत ही कहते रहें। आप स्वयं इसका प्रयोग करके देखिए। स्वयं अपना निरीक्षण कीजिए और देखिए। 'मैं यह शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ - यह आपकी वाणी कहेगी, मन भी मानेगा और बुद्धि तर्क द्वारा स्वयं को समझाने का प्रयत्न करेगी; परन्तु दूसरी ओर बुद्धि विवेक-प्रक्रिया में लगी रहेगी।
इस अवस्था में आपको लगने लगेगा कि आप आत्मिक चेतना के स्तर तक पहुँच गये हैं; परन्तु उसी पल यदि कोई अचानक आ कर आपसे कहे - 'कैसे मूर्ख हो, व्यर्थ बैठे-बैठे समय नष्ट कर रहे हो, काम क्यों नहीं करते चल कर', तो आप तुरन्त क्रोध से उत्तेजित हो उठेंगे। वेदान्त गायब हो जायेगा और बुद्धि क्रोध के, उस क्रोध के अधीन हो जायेगी जो दीर्घकालीन आदत के अनुसार मन में अनायास उत्पन्न हो गया है। जब वह व्यक्ति आपकी ओर देख कर आपको घूरने लगता है और आपको मूर्ख कहता है, आप तुरन्त यही निष्कर्ष निकालेंगे कि वह आपको मूर्ख कह रहा है।
वह शरीर की ओर संकेत करता हुआ एक नाम और एक रूप को सम्बोधित करता हुआ कहता है-"अमुक आप मूर्ख हैं।" और अमुक, अमर आत्मा, सच्चिदानन्द, मन और शरीर से परे, द्वन्द्वातीत लड़ने के लिए तुरन्त उठ खड़ा होता है। आपका मन विक्षिप्त है। वह उत्तेजित है और सोचता है कि 'इस आदमी से कैसे बदला लूँ?' क्रोध भड़कने लगता है, मन उत्तेजित हो जाता है और आपका मन कहता है कि जा कर उसकी नाक पर जोर से घूँसा मारें। आप पूर्णरूपेण भूल जाते हैं कि आप सर्वदा शान्ति और आनन्द से पूर्ण सच्चिदानन्द आत्मा हैं कि आप शरीर और मन, बुद्धि, नाम, रूप आदि से परे परिपूर्ण अद्वैत हैं। अतः आपको कौन अपशब्द कह सकता है। आपकी भावना होगी, 'मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं है। केवल सच्चिदानन्द है। मैं आनन्द, आनन्द, आनन्द हूँ।'
क्रोध की यह अकस्मात् आयी लहर जो सौन्दर्य को कुरूपता में, अहिंसा को हिंसा में, आपकी उच्च प्रकृति के सत्य को आपकी निम्न प्रकृति के मिथ्यात्व में परिवर्तित कर दिव्य जीवन के प्रमुख तीनों मूल्यों अर्थात् सत्य, शुचिता और दया का निषेध कर देती है तथा आपकी सच्चिदानन्द आत्मा को सर्वथा विपरीत रूप दे देती है- 'मल' है। यह प्रमुख विकार है। क्रोध, लोभ, काम, स्वार्थपरता, अहं, भ्रम, देहासक्ति, नाम, रूप, वासनाएँ, ईर्ष्या, द्वेष आदि ये सब मानव-स्वभाव के मल हैं। ये बहुधा प्रकट हो कर मन को अपने अधीन कर लेते हैं। मन इनसे ही भर जाता है और आपका सच्चिदानन्द स्वरूप ढक जाता है, वह विस्मृत हो जाता है और तुच्छता, बेईमानी, असहनशीलता, घमण्ड तथा यह विचार कि 'उसने मुझे ऐसा कहने की कैसे हिम्मत की'-मन में आ जाता है।
इन्हें मल कहते हैं। ये मानव-जीवन के मूलभूत विकार हैं। यदि आप चेतना के उच्च स्तर पर पहुँचना चाहते हैं, तो आपको उन्हें नष्ट करना होगा। ये विकार मानव-मन को निरन्तर अशान्त किये रहते हैं और जब तक ये हमारी प्रकृति में पूर्णरूप से सक्रिय हैं, तब तक सर्वशुद्ध आंत्म-भाव हमारी चेतना में कैसे आविर्भूत हो सकता है?
अतः श्री शंकराचार्य जी ने कहा है कि एक बाधा अनात्म भाव-रूपी मल है। ये मलिनताएँ मन को सर्वदा अशान्त और क्रियाशील रखती हैं; उसे कभी भी शान्त तथा स्थिर नहीं रहने देतीं। अतः जब तक ये मलिनताएँ मन को प्रतिक्षण अनाध्यात्मिक कर्मों की ओर ले जाती रहेंगी, तब तक मन किस प्रकार अन्तर्मुखी, शान्त, स्थिर, एकाग्र और ध्यानावस्थित हो सकता है? कैसे आप परम सत्ता पर चिन्तन का अखण्ड प्रवाह बनाये रख सकते हैं?
मलिनताओं के कारण मन रजस् एवं तमस् जैसे निम्न गुणों से भर जाता है और परिणामतः निरन्तर अशान्त, बहिर्मुखी तथा विक्षिप्त रहता है। यह दूसरी बाधा है जिसे 'विक्षेप' कहा जाता है। इसे भी जीतना होगा।
मन की और गहराई में तीसरा कारण निहित है। आप अपने दिव्य स्वरूप को बिलकुल भूल जाते हैं और केवल एक क्रोधी प्रतिशोध लेने को कटिबद्ध व्यक्ति रह जाते हैं। जिसके कारण आप अपने उच्च दिव्य स्वरूप को भूल जाते हैं, वह आपके आत्मिक चैतन्य और आपकी देहगत और मनस्गत चेतना के बीच एक अविभेद्य आवरण है। इसी के कारण चेतना क्रोध-तरंग के साथ एक हो जाती है-नाम-रूप के संग ही नहीं, मन और मन की वृत्तियों से तादात्म्य कर लेती है। यह एक ऐसा रहस्यमय आवरण है जो आपको आपके उच्च स्वभाव का ज्ञान नहीं होने देता। आपकी सत्ता की गहराइयों में यह सदा विद्यमान रहता है। यह आपकी चेतना की आन्तर गहराइयों पर आवरण है।
मल, विक्षेप तथा आवरण-इन तीनों बाधाओं का अतिक्रमण करना होगा। मानव-स्वभाव की निम्न कोटि की मलिनताएँ-विकार- 'मल' हैं। मन की निरन्तर अशान्त और उत्तेजित रहने की प्रवृत्ति 'विक्षेप' कहलाती है। विक्षेप के कारण मन एकाग्र और अन्तर्मुख नहीं हो पाता। 'आवरण' तत्त्वतः अविद्या का, मूल अविद्या का ज्ञान या अनुभूति न होना है। यह आवरण आपको छुपा देता है। अविद्या का यह आवरण देह-मन-अध्यास से होता है। अविद्या का यह आवरण मन के अन्दर देह और मन के अध्यास (देह और मन को चेतना समझ लेने) के रूप में वर्तमान है। उक्त तीनों ही बाधाओं के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों का अतिक्रमण करना होगा।
स्थूलता देहाध्यास है। इसके अन्तर तमस् और तमस् के अन्तर रजस् तथा अन्तरतम सत्त्व का आवरण है। आप इसे सत्त्व क्यों कहते हैं? इसीलिए न कि यह ज्ञान है! वस्तुतः इसमें ज्ञान है। इसमें ज्ञान का अभाव वैसा नहीं होता जैसा गहरी निद्रा में होता है। गहरी निद्रा पूर्ण अचेतनता की, अज्ञानता की अवस्था होती है, यद्यपि उस अवस्था में आप कुछ भी जान नहीं पाते। यहाँ इस अवस्था में आप जानते हैं, आपको कम-से-कम इसकी चेतना है कि आप अमुक और अमुक हैं और अभी आपका अपमान हुआ है। आप कुछ तो जानते ही हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि आप जो-कुछ जानते हैं, पूर्णतः गलत जानते हैं। ज्ञान अवश्य है, परन्तु इस ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है; क्योंकि यह मिथ्या ज्ञान है, उलटा-पुलटा ज्ञान है। इसमें आप जो नहीं हैं, अपने उस मिथ्या रूप को ही पूरी सच्चाई से मानने लगते हैं। अतः इस अवस्था में ज्ञान और चेतना रहती है; परन्तु वह अविद्या (अज्ञान) से आच्छादित रहती है। यह ज्ञान और चेतना की अवस्था है और सत्त्व से उद्भूत है। चेतना पर सत्त्व का आधार है। समस्त चेतनापरक ज्ञान सत्त्व है। परन्तु यह ज्ञान अविद्या-जनित है; अतः अज्ञान कहा जाता है। इसके स्थान पर आपको परम सत्य का ज्ञान, ब्रह्मज्ञान स्थापित करना चाहिए।
इस प्रकार तमस्, रजस् एवं सत्त्व-मल, चंचल वृत्तियाँ तथा अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान या विस्मृति का आवरण ये तीन बाधाएँ हैं जिन्हें विधिवत् क्रमशः सोपान-प्रति-सोपान पार करना है और इन तीनों बाधाओं को पार करने पर तब अचानक आप देखेंगे-ज्ञानोदय, आत्मज्ञान का प्रोज्ज्वल प्रकाश! अपने असली स्वरूप के समक्ष होंगे और तब होगा इन्द्रियातीत अनुभव, महा-अनुभव!
मूल अविद्या-मल का निवारण उसके प्रतिकूल भावना से ही हो सकता है। अन्धकार को दूर करने हेतु आप क्या करते हैं? न आप पोंछने के लिए कपड़ा लाते हैं, न झाड़ने के लिए झाडू, न बटोर कर रखने के लिए बोरा आदि। आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। अन्धकार को नष्ट करना है तो उसके विपरीत तत्त्व को-प्रकाश को लाना होगा। ज्यों-ही उसका भावात्मक (Positive) विपरीत, प्रतिकूल गुण उपस्थित हुआ, अभावात्मक (Negative) गुण अन्तर्धान हो जायेगा; क्योंकि अभावात्मक गुण का कोई आधार नहीं होता। अभावात्मक गुण की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती। इसे भली-भाँति याद रखिए।
अभावात्मक गुण अपनी अलग सत्ता नहीं रखते। उनमें वस्तुतः शक्ति होती ही नहीं, वे केवल भावात्मक गुणों का अभाव मात्र हैं। जब हम कहते हैं कि वह महा मिथ्यावादी है, तो इसका आशय होता है कि उसमें सत्यता नहीं है। झूठ और मिथ्यात्व अपने में कोई तत्त्व नहीं हैं, केवल सत्यता का अभाव है और जब किसी व्यक्ति में सत्यता का अभाव होता है, तो उसे झूठा कहा जाता है। वह कहता है- "अच्छा, अब मैं भी तुम्हें सच्चा बन कर दिखा दूँगा।" और सत्य उसके जीवन में जिस क्षण आ जाता है, उसे मिथ्यावादी कहना कोई अर्थ नहीं रखता।
घृणा भावात्मक गुण नहीं है। घृणा जैसी कोई चीज नहीं है। कोई काली छाया है। जो आपको घेरती है। इसका अर्थ है-न प्रीति को कोई स्थान है, न दयालुता को। अतः यह स्थिति प्रीति के अभाव की सूचक है। और जो प्रेम एवं सहानुभूति प्रवण होता है, उसमें घृणा-भाव नहीं होता। प्रेम के आते ही घृणा विलुप्त हो जाती है; क्योंकि जो भावात्मक है, वह वास्तविक है और जो अभावात्मक है, वह अवास्तविक (मिथ्या) है। जब भावात्मक गुण का विकास किया जाता है, तो अभावात्मक गुण निःशेष हो जाता है।
इसी प्रकार हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज कहते थे कि दिव्य गुणों का विकास कुरुचिपूर्ण विकारग्रस्त स्वभाव के रूप में व्यंजित दिव्य गुणों के अभाव को दूर करने की विधि है। कुरुचिपूर्ण स्वभाव से पता चलता है कि कुछ गुण जो आवश्यक और वांछनीय थे, उनका विकास नहीं हुआ है। उनका अभाव है। जिस क्षण वे प्रकट होंगे, व्यक्ति में परिवर्तन आ जायेगा। वह आज जैसा नहीं रहेगा; क्योंकि अभी उसमें कुछ आवश्यक गुणों की कमी है। उसमें कोई भावात्मक गुण ही नहीं है-बस, वांछित भावात्मक गुण उसमें नहीं है। हमारी नैतिकता की बुनावट में रिक्त स्थान है जिसे भरना है। अतः उचित गुण जिस क्षण भी आ जाता है, सब-कुछ पूर्ण हो जाता है।
अतः याद रखिए कि गुणों का विकास करना आध्यात्मिक अनुशासन तथा दिव्य अनुभव की ओर ले जाने वाले आत्मानुशासन का ही मुख्य अंश है। दिव्य गुणों का विकास एक प्रकार से नींव डालना है। यदि आप अपने खरीदे हुए जंगल के भूमि- खण्ड को फूलों का बगीचा बनाना चाहते हैं, तो आरम्भ में ही आप सर्वप्रथम फूल के बीज नहीं बोयेंगे। ईसा ने बाइबिल में क्या कहा है-आप जानते हैं? यदि आप झाड़ियों तथा कण्टकों के बीच में बीज बो देंगे, तो अंकुरित और विकसित होते समय वे भूमि के अनुकूल न होने के कारण घुट जायेंगे और मर जायेंगे। अतः पहले आप भूमि तैयार कीजिए। सर्वप्रथम आप जंगली घास, खरपतवार, काँटे आदि उखाड़ डालें। फिर कंकड़, पत्थर तथा ढेले निकाल कर भूमि को निर्मल बनायें।
अतः उन वस्तुओं को, वृत्तियों को निकाल बाहर करना जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है और जो आपकी वांछित अवस्था के प्रतिकूल हैं, आपकी तैयारी का आवश्यक अंग है। व्यर्थ की वस्तुओं से छुटकारा पायें। अदिव्य, अनाध्यात्मिक, अधम, क्रूर तथा पाशविक वृत्तियाँ जैसे लोभ, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थपरता, अहंकार, दम्भ और आसक्ति को नष्ट करें। इन सबको नष्ट करना होगा। तभी आप अपने हृदय-उपवन में श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज द्वारा बताये अठारह गुणों के पुष्प लगा सकते हैं और तब ही आप भागवत जीवन की अवस्था को पा सकेंगे। भागवत जीवन के बाद स्वच्छता का स्थान है। इसमें एक से अधिक अर्थ निहित हैं। दिव्य गुणों के विकास हेतु हृदय में बहुत अधिक उत्साह होना चाहिए।
गीता के सोलहवें अध्याय में इन गुणों का अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से वर्णन हुआ है। 'मैं यह देह और यह मन नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ" -इसका अनुभव करना चाहते हो तो धर्माचरण करो। सद्गुणों का आचरण करो। अपनी निम्न प्रकृति की मूल-विकृतियों को दूर करो जो सदैव ही हमारे स्वभाव का एक अभिन्न अंग बन कर रहती आयी हैं। वस्तुतः उनकी कोई सत्ता नहीं। सद्वृत्तियों का अभाव होने से ही वे प्रतीत होती हैं।
अपने हृदय-उपवन में गुणों के पुष्प विकसित कीजिए। सद्गुणों के विकास से ही मन की चंचलता, उग्रता, व्यग्रता तथा अशान्ति दूर की जा सकती हैं। प्रार्थना तथा अन्य आभ्यन्तरिक प्रक्रियाओं द्वारा अज्ञान का आवरण चीर कर फेंका जा सकता है। सघन ध्यान और आत्मिक जिज्ञासा, विवेक, आत्म-विश्लेषण तथा अविरल अध्यात्म-चिन्तन द्वारा आप परम चेतना की, आत्म-बोध की अवस्था को पा सकेंगे। तब आपको कैसा अनुभव होगा? आप कैसा अनुभव करेंगे! क्या कहेंगे? उन क्षणों के, उस अध्यात्म-चेतना के, दिव्य चेतना के महा-अनुभव को- 'मैं सच्चिदानन्द हूँ', इस अनुभव को किस प्रकार, किन शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे?
११. छात्र-जीवन का महत्त्व
विद्यार्थी-काल के परम मूल्य को न आँका जा सकता है, न उसका वर्णन किया जा सकता है। विद्यार्थी-जीवन सर्वाधिक मूल्यवान् है। युवा-अवस्था सर्वोत्तम काल है। इस काल में आपने जीवन का उपयोग किस प्रकार किया है, वही आपके भावी जीवन का निर्धारण करेगा। आपका भावी सुख, सफलता, सम्मान, प्रसिद्धि और यश इस काल के जीवन यापन की विधि पर निर्भर करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियो! स्मरण रखिए कि इसी वर्तमान अवधि में ही आप अपना भविष्य बना रहे हैं। आपके जीवन के प्रथम सोपान का यह अद्भुत समय उसी प्रकार से है जैसे कुम्हार के हाथ में मुलायम गीली मिट्टी। कुम्हार उसे कुशलतापूर्वक मनोवांछित उचित स्वरूप और आकार देता है। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन को, अपने चरित्र को, शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति को अर्थात् अपने समस्त स्वभाव को जैसा आप चाहते हैं, ढाल सकते हैं। और इसे आप अभी कर डालिए।
भाग्यशाली युवको! इस महा-कर्तव्य को समझो और स्वयं को ढालने के इस अद्भुत अधिकार का अनुभव करो। इसमें साहसपूर्वक जुट जाओ। ईश्वर की कृपा-दृष्टि आप पर है। वह सदैव आपकी सहायता तथा पथ-प्रदर्शन को तैयार है। मेरी कामना है, आप महान् बनें। संसार को आपसे आशाएँ हैं। आपके अग्रज भी आपसे आशा रखते हैं। युवा का आशय है स्वयं में दृढ़ आस्था रखते हुए अपने आशापूर्ण निश्चय, संकल्प और सदुद्देश्यों को आत्म-संस्कार के सुन्दर कार्य में लगा देना। इसके द्वारा सचमुच ही आपको परम सन्तोष और परिपूर्णता मिलेगी। केवल आपको ही नहीं प्रत्युत उनको भी जो इसके आकांक्षी होंगे। अपने जीवन को आकार देना वास्तव में आपके ही हाथ में है।
धर्माचरण करो, धर्म में निरन्तर संलग्न रहो। धर्मनिष्ठ रहो। सदैव धर्म के साकार रूप बन कर उद्भासित रहो। अच्छाई को अपना अंग बना लो। युवा-अवस्था इस महान् प्रक्रिया के लिए ही है। छात्र-जीवन इस प्रक्रिया का सक्रिय विकास और पूर्ति है। तुम्हारे समय की यह अवधि जीवन की महत्त्वपूर्ण और अपरिहार्य इस प्रक्रिया के लिए पूर्ण अनुकूल और उपयुक्त क्षेत्र उपस्थित करती है। छात्र-जीवन का यही विशेष महत्त्व और यही परम मूल्य है। यह दिव्य व्यक्तित्व के विकास का प्रतीक है। यही आत्म-विकास है। यही आत्म-निर्माण है।
सफल जीवन के सही भाव और अर्थ को समझने का प्रयत्न करो। जब तुम सफलता की बात जीवन के सन्दर्भ में करते हो, तो इसका आशय यह नहीं है कि तुम जो-कुछ करो, सबमें सफलता पाओ और न सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाना या इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेना ही इसका अर्थ है। यश या पद पा लेना अथवा अधुनातन सभी प्रकार के फैशनों का अनुकरण करते हुए स्वयं को अति-आधुनिक दिखाना भी इसका आशय नहीं है। वास्तविक सफलता का सार है आप अपने को कैसा बनाते हैं? यह जीवन का वह आचरण है जिसे आप विकसित करते हैं, वह चरित्र है जिसे आप निर्मित करते हैं और तदनुरूप आप बन जाते हैं। समस्त जीवन यापन का यही केन्द्रीय अर्थ है। अतः आप देखेंगे कि यह आवश्यक तथ्य जीवन में सफलता पाने का प्रश्न उतना नहीं है जितना जीवन को सफल बनाने का है। ऐसा सफल जीवन वही है जो आदर्श पुरुष को, साधु पुरुष को पैदा करे। आपकी सफलता इससे नहीं मापी जाती है कि आपको कितना मिला, बल्कि इससे मापी जाती है कि आप कैसे बने हैं, आपकी जीवन-पद्धति कैसी है तथा आप कैसा कर्म करते हैं। इस पक्ष को चिन्तन में लाइए और परम सुख प्राप्त कीजिए।
हमारी इस महान् संस्कृति में जीवन की चार अवस्थाएँ मानी जाती हैं- प्रारम्भिक अवस्था, विकास-अवस्था, पुष्पण-अवस्था और फलवती अवस्था। इन चारों अवस्थाओं को क्रमशः तैयारी का काल, साधना-काल, प्रगति-काल तथा पूर्णता का, फल-प्राप्ति का काल भी कह सकते हैं। प्रथम अवस्था की सुव्यवस्था पर ही अन्य तीनों अवस्थाओं का समुचित विकास निर्भर करता है। आप लोगों का यह जीवन सही और सफल जीवन हेतु प्रारम्भिक तैयारी की अवस्था है। इसी कारण इस छात्र-जीवन का परम मूल्य और विशेष महत्त्व है। यह कृषक द्वारा खेत में हल चलाने और बीज बोने जैसा है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि भविष्य में जो जिस प्रकार की फसल पाना चाहता है, उसके सन्दर्भ में इस जीवन का क्या अभिप्राय और महत्त्व है?
इसके अतिरिक्त आप जो महत्त्वपूर्ण भवन निर्माण करना चाहते हैं, यह काल उसकी नींव डालने के समान है। यदि यह भवन आपके लिए बहुत ही महत्त्व का है, तब सोचिए कि उचित नींव डालना आपकी दृष्टि में कितना महत्त्वपूर्ण होगा? भवन की सुदृढ़ता और टिकाऊपन निश्चय ही नींव पर निर्भर करता है। आप इस नींव की अवस्था में हैं। आप बुद्धिमत्ता से सही तरीके से इस तरह तैयारी करें कि उसकी परिणति आपके परम कल्याण, परम हित तथा स्थायी सन्तोष और सुख में हो। छात्र-जीवन की सम्पूर्ण अवधि में आपका ध्यान इसी लक्ष्य पर लगा रहे और उसकी पूर्ति हेतु आप सोत्साह कार्यरत रहें।
हमारी संस्कृति में इस अवस्था को ब्रह्मचर्याश्रम या विद्यार्थी-जीवन कहते हैं। यहाँ आप केवल इतिहास, भूगोल, अंकगणित आदि विषयों का ही ज्ञान अर्जित नहीं करते, प्रत्युत मानव-स्वभाव का, सम्यक् व्यवहार का, आत्मानुशासन का, शुद्ध मानसिक विकास का, धर्म का, मनुष्य के कर्तव्यों तथा आपके, जगत् के और ईश्वर के बीच परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। मैं दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था का वर्णन संक्षेप में करूँगा। तदुपरान्त उस आवश्यक प्रश्न को लूँगा कि किस प्रकार आप अपनी इस युवावस्था को अत्यधिक उपयोगी बना सकते हैं।
दूसरी अवस्था जिसे आप गृहस्थाश्रम के नाम से जानते हैं, वास्तव में वह अवस्था है जब व्यक्ति में धर्म-सम्बन्धी अपने समस्त ज्ञान को-उचित व्यवहार, सम्यक् कर्तव्य, गुण, आचरण, ईश्वर और मानव के पारस्परिक सम्बन्ध की परिपूर्णता से सम्बन्धित ज्ञान को-व्यवहार में, क्रिया में लाने की धुन उत्पन्न हो जाती है। इसी काल में विद्यार्थी-जीवन में की हुई प्रारम्भिक तैयारी की जाँच और परीक्षा विविध परिस्थितियों, अनेकानेक प्रलोभनों, समस्याओं और स्थिति-परिवर्तन द्वारा की जाती है। यदि विद्यार्थी-काल में तैयारी कुशलतापूर्वक हुई है, तो गृहस्थाश्रमी अपने आदर्शों पर स्थित रह सकता है और इस अवस्था में हर प्रकार के प्रलोभनों, बाधाओं, कठिनाइयों और परीक्षाओं की कसौटियों पर खरा उतर कर अपने आन्तरिक महत्त्व को प्रमाणित कर सकता है, अपने आत्म-बल को बढ़ा सकता है और अपने व्यक्तित्व में अतिरिक्त प्रौढ़ता ला सकता है। आत्म-बल, धर्म और आदर्श व्यवहार वाला ऐसा व्यक्ति समाज के लिए वरदान, परिवार की प्रतिष्ठा और अपने निकटवर्ती लोगों के लिए प्रेरणादायक दृष्टान्त बन जाता है। उसका जीवन सदाशयता, शुद्धता और धर्म के लिए उत्साह उत्पन्न करता है।
वानप्रस्थ नामक तीसरी अवस्था में वह और प्रगति करता है तथा अपने ज्ञान में, अनुभवों में तथा अपने विकसित गुणों में शेष जन-समाज को उसके हितार्थ सहभागी बनाता है। युवा जनों के लिए वह पथ-प्रदर्शक, गृहस्थों के लिए प्रेरणादायक परामर्शदाता तथा सभी का निःस्वार्थ सेवक बन जाता है। तीसरे आश्रम का यही आशय और यही आदर्श है। प्रथम अवस्था की कुशल तैयारी, दूसरी अवस्था में दत्तचित्त हो कर व्यावहारिक जीवन यापन करने तथा तीसरी अवस्था में शेष जनों को निःस्वार्थ भाव से सहभागी बनाने के फलस्वरूप प्राप्त चतुर्थ अवस्था संन्यास की आती है। इसमें मन शान्त, स्थिर और शुद्ध हो जाता है तथा हृदय निष्काम और एषणाओं से मुक्त हो कर पूर्ण आत्म-संयमी और धर्मनिष्ठ हो जाता है। संन्यास-जीवन की यह आदर्श अवस्था उससे पूर्व तीनों अवस्थाओं को सम्यक् रूप में व्यतीत करने का फल होती है। इसमें व्यक्ति स्वतः ही अनायास ईश्वर-चिन्तन में लीन हो ईश्वर-अनुभव की ओर अग्रसर होता है। वह आन्तरिक अध्यात्म-जीवन की, परम शान्ति और आत्मिक आनन्द की प्रचुर फसल काटता है और उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसके लिए उसे यह मानव-जन्म मिला है। परन्तु यह तभी सम्भव है, जब व्यक्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इस विद्यार्थी-जीवन में सही व्यवहार एवं उचित प्रयत्न से श्रमपूर्वक इसके योग्य बना ले।
आपको क्या करना है? कैसे जीवन जीना है? क्या पाने का प्रयत्न करना है? कौन से तथ्य हैं जो विद्यार्थी-जीवन को सुघढ़ सुन्दर बनाने के लिए आवश्यक हैं? ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो आपके समक्ष हैं। क्या कभी आपने इन प्रश्नों को स्वयं से पूछा और समाधान पाया? अब कृपया ध्यान दे कर सुनें।
आपको अपने मन में एक स्पष्ट धारणा बनानी चाहिए कि आप अपना विकास और अपने को पूर्ण किस प्रकार करना चाहते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, उसकी स्पष्ट कल्पना आपके मन में होनी चाहिए। इसके द्वारा आपको जीवन का स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य प्राप्त होगा। बिना इस प्रकार के लक्ष्य के आप सशक्त रूप में प्रगति नहीं कर सकेंगे। आप विभिन्न दिशाओं से आकर्षित किये जायेंगे, ध्यान भंग होगा, मन विचलित होगा और बहुत सी शक्ति व्यर्थ में नष्ट होगी। यदि आपका लक्ष्य सुनिश्चित है या इसी प्रकार के उद्देश्य निश्चित हो चुके हैं, तो आप इनसे बच कर निकल सकते हैं।
अब जब कि आपका जीवन एक निश्चित दिशा ले चुका है, वह किसी अन्य दिशा की ओर आकर्षित नहीं हो सकता। आपके मार्ग में कोई अव्यवस्था नहीं है। आपके मन में कोई और अस्पष्टता नहीं है। आप जानते हैं कि आपको क्या उपलब्ध करना है, जानते हैं कि किस दिशा में बढ़ना है। अतः आप यह भी जानते हैं कि जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या बांछनीय है और क्या अवांछनीय, क्या स्वीकार्य है और क्या अस्वीकार्य? इस प्रकार की निश्चितता आपको आन्तरिक बल देती है, आपकी संकल्प-शक्ति विकसित करती है और आपके व्यक्तित्व को सारवान् बनाती है। इसके पश्चात् आपके जीवन में नकारात्मक, सारहीन कोई वृत्ति रह ही नहीं जाती।
दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है जीवन के कार्यक्रम की समझदारी तथा विवेकपूर्ण ढंग से योजना बनाना जो आकांक्षित पथ पर बढ़ने तथा जीवन के लक्ष्य तक क्रमशः पहुँचने में सहायक हो। ऐसा कार्यक्रम विद्यार्थियों तथा नवयुवकों के समक्ष आने वाली समस्याओं तथा उनके जीवन में उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों से निबटने, दृढ़ मन से प्रलोभनों का सामना करने तथा उन पर विजय पाने तथा साहस और आत्म-विश्वास के साथ बाधाओं को पराजित करने के सम्बन्ध में एक कार्य-योजना भी प्रस्तुत करता है। यह सब करने की क्षमता आपमें पहले से ही विद्यमान है; परन्तु वह अन्तर्निहित अनभिव्यंजित है। उसे प्रकट करके क्रियाशील बनाना पड़ेगा। विवेकपूर्ण ढंग से बनाया हुआ कार्यक्रम और कार्य-योजना इन आन्तरिक क्षमताओं को प्रकटित करने और उनका विकास करने के लिए आवश्यक क्षेत्र तथा व्यावहारिक विधि प्रदान करती है। अपने जीवन के इस अद्भुत और रोचक काल को यापन करने के लिए मन को, उसके व्यवहार तथा आदत को तथा मन की आन्तरिक शक्तियों को नियन्त्रित करने वाले विधान को भली-भाँति समझ लेना बड़ा ही लाभदायक है। इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, उपयुक्त ग्रन्थों का अध्ययन कीजिए और इस प्रकार मन और उसकी क्रियाओं का मूलभूत ज्ञान प्राप्त कीजिए।
अब हम उस तथ्य पर आते हैं जिस पर आपके जीवन के कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन निर्भर करता है। वह है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्वास्थ्य के बिना न तो आप भली-भाँति अध्ययन कर सकते हैं, न चरित्र- निर्माण और न ही आप खेल-कूद की या सामाजिक क्रियाएँ कर सकते हैं, न ही घर के काम-काज में हाथ बँटा सकते हैं। स्वास्थ्य नियमित जीवन यापन है। यह आप जो-कुछ भोजन खाते-पीते हैं, उससे ही नहीं बनता प्रत्युत जो वस्तुएँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनसे बुद्धिमत्ता तथा सावधानीपूर्वक दूर रहने पर भी बनता है। स्वास्थ्य-रक्षा और बलवर्धन हेतु भोजन कीजिए, स्वाद के लिए न कीजिए। जीने के लिए तथा सेवा करने के लिए खाइए। खाने के लिए नहीं जीयें। सादा भोजन लीजिए। रात्रि में जल्दी सोयें और प्रातः जल्दी शय्या त्याग कर उठ जायें। स्वस्थ आदत डालिए। प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। खान-पान में सन्तुलन रखिए। खूब चबा कर खायें। अधिक न खायें। यदि भूख न हो, तो न खायें। जो वस्तुएँ आपके अनुकूल न पड़ती हों, उनका सेवन न करें।
इसके उपरान्त आप अपनी शक्ति को सुरक्षित रखें। उसका व्यर्थ के कार्यों में अपव्यय न होने दें। खूब बातें करना, गप्पें मारना, निरुद्देश्य इधर-उधर घूमना या मँडराना, चिन्तातुर रहना, बात-बात में क्रुद्ध हो जाना आदि ऐसे कार्य हैं जिनसे आपकी शक्ति का हास होता है। वे आपकी स्नायविक शक्ति का अपव्यय करती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी जो भी आदतें हानिकारक हैं, उन्हें त्याग दीजिए। धूम्रपान छात्रों के लिए अभिशाप है। अपनी संकल्प-शक्ति द्वारा ऐसी बुरी आदतों को जीत लो। आत्म-संयमी एवं इन्द्रियनिग्रही बनो। ब्रह्मचर्यनिष्ठ हो जाओ। पान खाने, धूम्रपान करने और सुँघनी आदि के सेवन की आदत छोड़ दो। सन्तुलित एवं व्यवस्थित जीवन जीओ। स्वास्थ्य की रक्षा करो। शक्ति को जमा करो। शारीरिक और मानसिक बल का विकास करो और इस प्रकार सफल जीवन की आधारशिला स्थापित करो।
संसार में सभी पदार्थों से अधिक मूल्यवान् चरित्र को समझें। पूर्णतः सत्यनिष्ठ रहें। अपनी वाणी को अशिष्ट और रुक्ष न बनायें। आपकी वाणी स्पष्ट, विनम्र और प्रमुदित करने वाली हो। वाणी सरस्वती है। यदि अशिष्टता और रुक्षता से वह अप्रसन्न हो गयी, तो आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अहंकार, अभिमान और स्वार्थपरता को दूर कर दीजिए। ये तीनों मानव जीवन के लिए अभिशाप हैं। ये अविद्या और लोभ से उत्पन्न होते हैं। अज्ञान (अविद्या) आपको अभिमानी और अहंवादी बनाता है। लोभ आपको स्वार्थी बनाता है। ये आपके लिए अपयश और दुःख का कारण बनते हैं और जीवन में असफलता लाते हैं। सादा जीवन यापन करते हुए तथा सभी परिस्थितियों में प्रसन्न मुद्रा में रहते हुए आप स्वार्थपरता और अहं-भाव को जीत सकते हैं। आपका जीवन और व्यवहार दूसरों के लिए सुखप्रदायक हो।
कुछ गुणों और सिद्धान्तों को अपनाइए और जीवन की समस्त क्रियाओं में उनसे जुड़े रहिए। अपने सिद्धान्तों को कभी न छोड़िए। गुणों से हट कर कभी दूर मत जाइए। वे गुण ही आपके सच्चे सहायक और मित्र होंगे। उनके कारण आपकी प्रगति निश्चित हो जायेगी और अन्ततः वे आपको परम सुख और सफलता प्रदान करेंगे। समय-समय पर उन सद्गुणों को आचरण में लाने का साधारण-सा संकल्प कीजिए। एक व्यक्तिगत डायरी रखिए और उसमें सावधानीपूर्वक अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या, दूसरों के प्रति अपना आचरण, वाणी और व्यवहार की टिप्पणी कीजिए। इससे आप जान सकेंगे कि आप कितने आगे बढ़े हैं, आपने क्या त्रुटियाँ की हैं और कहाँ आपको सँभलना और सुधरना है। ऐसी डायरी आपकी मित्र रहेगी। वह आपकी त्रुटियों को प्रकट करेगी और आपको नम्रता सिखायेगी। ईश्वर की प्रार्थना कीजिए कि वह आपको आन्तरिक शक्ति दे और आपका पथ-प्रदर्शन करे। उसके दिव्य नाम में असीम शक्ति है। अतः सर्वदा उसके नाम का जप कीजिए और उसे किसी भी परिस्थिति में न भूलिए।
महापुरुषों की जीवनी का चिन्तन कीजिए और उनके जीवन तथा उपदेशों से बल और प्रेरणा लीजिए। उनके जैसा स्वयं को ढालने का यत्न कीजिए। अपने मन में सदैव कोई महान् आदर्श रखिए और नित्य प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल तथा निशाकाल-सब समय उसका चिन्तन कीजिए। उसे सदैव अपने विचारों की, चिन्तन की पृष्ठभूमि बना लीजिए। तब आपका मन कभी भी सुस्त या खाली नहीं रहेगा। यह अति आवश्यक है। सम्यक् चिन्तन सजीवन की कुंजी है।
'जैसा बोओगे, वैसा काटोगे' कहावत की तरह आप जैसा सोचेंगे, वैसा ही बन जायेंगे। आप निरन्तर जिसका चिन्तन और भावना करेंगे, अन्ततः उसका अनुभव करेंगे और उसे उपलब्ध भी हो जायेंगे। आपके आन्तरिक विचार ही आपको बाह्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं और बार-बार किये गये कर्म आदत बन जाते हैं। ये आदतें आपके स्वभाव के स्थायी गुण बन जाते हैं और आपका यह स्वभाव ही आपका चरित्र-निर्माण करता है। आपका भविष्य और आपकी नियति आपके चरित्र के ही प्रत्यक्ष परिणाम हैं। इसे भली-भाँति समझ लीजिए और ध्यान में रखिए। इसी ज्ञान के अनुसार सोचिए और कर्म कीजिए।
आपके आन्तरिक विचार ही आपकी मूल नियति हैं। अतः अपने विचारों और भावनाओं पर दृष्टि रखिए। शिष्ट और सद्भावना सहित विचार कीजिए। आप श्रेष्ठ बन जायेंगे। आप महानता प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे। ग्रन्थों के अध्ययन से, शिक्षा और परीक्षा से, यहाँ तक कि प्रत्येक वस्तु से अधिक महत्त्वपूर्ण है जीवन में धर्म-भावना का विकास करना। सद्विचार, सत्कर्म और महान् चरित्र का विकास-ये सब आपको उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जायेंगे। आत्यन्तिक सुख का स्रोत यही है। इस पुण्य भूमि भारत माता के सच्चे सपूत होने के नाते जीवन का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करने का यह आदर्श तरीका है। मेरी कामना है कि आप अच्छे और महान् बनें!
१२. शुद्धता : योग-पथ-निर्मात्री
आपको तथा संसार के समस्त साधकों को मेरा प्रणाम और स्नेहपूर्ण शुभ कामनाएँ। मैं आपको इस वर्ष के लिए अपनी सर्वोत्कृष्ट शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ। आपका यह वर्ष, वर्ष के बारहों महीने आपके लिए सुख, शान्ति और उन्नति, सफलता तथा सम्पदा से पूर्ण हो कर आयें! गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज की कृपा से आप शान्ति, आनन्द और ज्ञान प्राप्त करें!
शुद्धता पूर्णता की प्रथम शर्त है। शुद्धता के बिना किसी प्रकार की भी आध्यात्मिक उन्नति सम्भव नहीं है। शुद्धता वह नींव का पत्थर है जिस पर साधक अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करता है। शुद्ध मनस् ही आपको ईश्वराभिमुख कर सकता है। अन्तर से शुद्ध व्यक्ति ही योग-पथ पर दृढ़तापूर्वक चल सकता है। शुद्धता व्यक्ति में आमूल परिवर्तन कर देती है और व्यक्ति अपनी निम्न प्रकृति से उठ कर दिव्य प्रकृति का बन जाता है।
परमात्मा सर्व शुद्ध और निरंजन है; कालिमा, मलिनता-रहित है; अतः उसका अनुभव शुद्ध मन से किया जा सकता है। उसका साक्षात्कार व्यक्ति की निर्मल अन्तर चेतना ही कर सकती है। मन या बुद्धि द्वारा उसका अनुभव, उसके असली रूप का अनुभव नहीं हो सकता। वह इन्द्रियातीत है। वह न बुद्धि से जाना जा सकता है, न मन से; क्योंकि मन और बुद्धि से जानने में कुछ प्रक्रियाओं का सन्निवेश होता है और परमात्मा प्रक्रियाओं की उपज नहीं है। अतः मन और बुद्धि रूप जो साधन हमें प्राप्त हैं, उन साधनों से परमात्मा उपलब्ध नहीं हो सकता। बुद्धि मन का अंश है।
ईश्वर को एक-दूसरे ही स्तर द्वारा जाना जा सकता है और हमारी सत्ता का वह स्तर हमारा निज स्वरूप है, आध्यात्मिक नेत्र है जिसे दिव्य नेत्र भी कहा गया है। जब तक हमारा वास्तविक स्वरूप मल से आच्छादित है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक अन्तर्चक्षु या ज्ञानचक्षु नहीं खुलते, तब तक दिव्य साक्षात्कार नहीं हो सकता। अतएव हम विचार कर अन्त में इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ईश्वर दृश्य सत्ता नहीं है। ईश्वर ऐसी सत्ता नहीं है जिसे जाना जा सके। उसको जाना नहीं जा सकता। उसका अवबोध नहीं हो सकता। हमारे धर्मग्रन्थ कहते हैं कि उसका अनुभव केवल शुद्ध मनस् कर सकता है। उसका केवल तत्त्वतः ही अनुभव हो सकता है। वह जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल सम्यक् उपासना द्वारा, शुद्ध मन द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इसको पाने का कोई उपाय नहीं है।
ईश्वर के निकट से निकटतर पहुँचने के लिए, समीप से समीपतर आने के लिए उपासना कीजिए। उपासना का अर्थ है ईश्वर की अति-समीपता। अतः यदि आप पूर्णत्व चाहते हैं, तो सम्यक् उपासना द्वारा परमात्मा के निकट से निकटतर आ कर उसे अनुभव कीजिए। अन्तिम स्तर पर उसका वास्तविक अनुभव आपको तभी होगा, जब आप तदाकार हो जायेंगे। उपासना के चरमोत्कर्ष पर पहुँच कर आप परम अनुभव प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान और समाधि उपासना की उच्चतम कोटि है। ईश्वर की सर्वोत्तम उपासना गहरे ध्यान में पूर्णतः लीन हो कर उससे सीधा सम्बन्ध जोड़ना है।
उपासना के विविध प्रकार हैं। बहिर्मुखी उपासना, प्रतीकोपासना आदि से आरम्भ हो कर इन उपासनाओं की क्रमशः कई कोटियाँ हैं। उपासना का निम्नतम रूप, तामसिक उपासना भी ईश्वरोपासना का ही एक प्रकार है। बहिर्मुखी, नैष्ठिक और प्रतीकात्मक उपासना से ले कर आप उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उपासना की अनेक कोटियाँ पार करके अन्त में अपनी अन्तर्चेतना में गहरे ध्यान की तन्मयता की उच्च कोटि की उपासना में लीन हो जाते हैं। यह समाधि है। ध्यान उपासना का सर्वोच्च रूप है और यह परम उपासना अन्त में समाधि में पर्यवसित हो जाती है। ज्ञान और समाधि की अवस्था में चेतना दिव्य हो जाती है, भौतिक तत्त्वों से विमुख हो पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाती है। उस नितान्त शुद्ध अवस्था में ईश्वर की सत्ता से मिल कर जब आप उसका अनुभव प्राप्त करते हैं और उसी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब कहा जाता है कि आप 'वह' ही हो गये हैं। उसके स्वरूप में प्रविष्ट हो कर उसकी उपासना आरम्भ करके आप अन्त में 'उस' की ही जैसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उपनिषदों की प्रधान उद्घोषणा है : "ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति" - ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है।
योग की विविध प्रकार की, तरह-तरह की जितनी प्रक्रियाएँ हैं, वे सभी उपासना की उच्चतम अवस्था में आ कर एक हो जाती हैं। उपासना की उच्चतम अवस्था है ध्यान में ईश्वर से सीधा सम्पर्क स्थापित कर लेना। वस्तुतः आप देखेंगे कि ध्यान-साधना एक ऐसा बिन्दु है जहाँ आ कर सब योग-साधनाएँ मिल जाती हैं। यद्यपि ये सभी भिन्न-भिन्न तरह से आरम्भ होती हैं, बढ़ती हैं तथा प्रगति और उन्नति भी भिन्न-भिन्न तरीके से करती हैं; परन्तु अन्त में आ कर ध्यान की अवस्था में एक हो जाती हैं। ध्यान समाधि में ले जाता है।
यदि आप पूर्व और पश्चिम के विभिन्न महान् रहस्यवादियों और विविध सन्तों का आध्यात्मिक इतिहास पढ़ें, तो आप जान सकेंगे कि बुद्ध और ईसा आदि के समान ही सब पैगम्बरों ने ध्यान किया और पूर्णत्व को उपलब्ध हुए। विश्व-भर के समस्त साधकों की आध्यात्मिक साधना में आप ध्यानोपासना को सामान्य रूप से सर्वत्र पायेंगे।
सभी धर्मशास्त्र काम, क्रोध और लोभ को साधक के शत्रु कहते हैं। क्रोध काम से सम्बन्धित है। क्रोध इस शरीर के स्नायविक मण्डल पर, मन पर और यहाँ तक कि उच्च आत्मा के आध्यात्मिक तन्तुओं पर भी महा-अत्याचार करता है। यह काम का ही विकार है। काम ही क्रोध में रूपान्तरित हो जाता है। ध्यानोपासना में ये बड़े बाधक हैं। अतः मन में से इन मलों को निकालना पड़ेगा। इन्हें किस प्रकार निकाला जाये, यह धर्मशास्त्र बताते हैं। अतः इन शत्रुओं पर विजय पाने के लिए व्यक्ति को और कहीं सहायता हेतु जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों विकार निम्न गुणों अर्थात् रजस् और तमस् की उपज हैं। अतः अपने में सत्त्व को भर कर सम्पूर्ण जीवन को सात्त्विक बना लेने पर हम इन शत्रुओं का विनाश कर सकेंगे ।
अपने अन्तर से इन विकारों को निकाल फेंकने का एकमात्र उपाय है जीवन को हर दृष्टि से सात्त्विक रूप में यापन करना। इस प्रकार का सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए व्यक्ति काम और क्रोध से छुटकारा पा जायेगा। निम्न कोटि के इन विकारों के चंगुल से मुक्त होने के लिए साधक को यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। पाने योग्य कोई भी वस्तु तब तक प्राप्त नहीं होती, जब तक उसको पाने के लिए उतना ही कष्ट न भोग लिया जाये। जब तक हम कठिन प्रयत्न नहीं करेंगे, पसीना नहीं बहायेंगे, तब तक स्थायी आदर्श को उपलब्ध नहीं कर सकते।
युवा साधकों को भी देर-सवेर इस तरह की सब स्थितियों से गुजरना ही पड़ेगा। इन परीक्षाओं का उन्हें वैसी ही एक-सी दृढ़ता से सामना करना चाहिए जैसी दृढ़ता से अपने साधना-काल में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने किया था। पूर्णता का पथ किसी-न-किसी समय कठिन तपस्या और अडिग सहनशीलता की अपेक्षा करता ही है। सभी जिज्ञासु आत्माओं का, जो आत्म-साक्षात्कार के सच्चे आकांक्षी थे, यही अनुभव रहा है और उन्होंने ऐसा अनुभव करके दम्भ और भूलों से भरे इस जगत् से मुँह मोड़ लिया। सत्य ही है कि मनुष्य और ईश्वर का सम्बन्ध परीक्षा और प्रतिकूलता की भट्ठी में तपा कर ही जुड़ता है।
यदि कोई पूर्णत्व प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए समस्त कठिनाइयों को साहस के साथ सहन करना और अन्त तक हिम्मत न हारने का सुदृढ़ संकल्प अत्यावश्यक है। नये वर्ष के शुभारम्भ पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको उत्तम स्वास्थ्य, जीवन में पूर्ण सफलता और उच्चतम आध्यात्मिक वैभव प्रदान करे! यही प्रार्थना मैं अपने गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के पुनीत चरणों में भी करता हूँ।
१३. वास्तविक आनन्द का रहस्य
इस भ्रम-जाल से उत्पन्न इच्छाएँ और कामनाएँ मन की शान्ति नष्ट कर देती हैं। शान्ति-रहित मन सुखी कैसे रह सकता है? सुख मन की शान्ति पर निर्भर करता है। शान्त, अचंचल मन में ही सुख उत्पन्न होता है; क्योंकि असली सुख आपकी अन्तर्मुखी अवस्था है। भाग्य या अभाग्यवश इसकी अभिव्यंजना का माध्यम केवल बुद्धि और मन हैं। अगर ये दोनों ही माध्यम उत्तेजना की ऐसी दशा में हों कि वे उमड़ते हुए इस आन्तरिक आनन्द की अभिव्यक्ति का उचित माध्यम न बन सकें, तब उनकी दशा अनुपयुक्त तथा प्रतिकूल हो जायेगी। मन और बुद्धि में शान्ति और निश्चलता होने पर ही आन्तरिक सुख की अनुभूति हो सकती है।
आपकी शान्ति और सुस्थिरता का अपहरण इच्छाओं और कामनाओं की भावना द्वारा होता है और यह भावना उस मूलभूत त्रुटि से उपजती है जिसके कारण आप समझते हैं कि सुख विषयों पर निर्भर है। यही त्रुटि है जिसमें आप जीना आरम्भ करते हैं। शैशवावस्था में ही बालक तो बता दिया जाता है कि सुखमय जीवन का अर्थ है कहीं-कहीं आना-जाना, करना, वस्तुओं को लेना आदि। और बालक इसी भ्रम के साथ बड़ा होता है और वयस्क बनने पर वह अपने से बाहर के पदार्थों के आश्रित रहने लगता है। यदि शैशवावस्था में ही बालक के मन में इस जगत् के वास्तविक स्वरूप का कण मात्र भी परिचय बैठा दिया जाये, तो कालान्तर में वह सुख और आनन्द की सघन फसल के रूप में तैयार हो जायेगा।
वस्तुओं के यथातथ्य मूल्यांकन का प्रयत्न करें। इस भूतल पर यदि सम्यक् जीवन यापन करना है, तो विषयों को परिमित महत्त्व दें। जीवन यापन के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। इसी उद्देश्य और लक्ष्य के लिए उनका उपयोग कीजिए; परन्तु अपने जीवन में उन्हें प्रधान मत होने दीजिए; क्योंकि तब वे आपके जीवन का पोषण करने की अपेक्षा जीवन की वास्तविक तृप्ति और सन्तोष का सारा रस एक आक्रामक की तरह शोषण कर लेंगे। आपका सुख इन विषयों के पास बन्धक रख दिया जा सकता है और तब वे परिमित उपयोगिता के विषय न रह कर सर्वाधिक महत्त्व के बन जायेंगे और इसी कारण वे आ कर आपको गरदनियाँ दे कर आप पर अधिकार जमाते हुए आपको अपना दास बना लेते हैं। विषयों को भली-भाँति समझना और उनका सही मूल्यांकन करना कि वे क्या हैं और किस प्रयोजनार्थ हैं-मानव-जीवन में बहुत महत्त्व रखता है। आपके जीवन के आन्तर राज्य पर वे (विषय) आक्रमण करें, तो उस समय आपको यही कहना पड़ेगा- 'यहीं तक, इससे आगे नहीं।'
जीवन की सादगी सुख का असली रहस्य है। अन्तर में छिपा आनन्द का अबाध अनुभव सादगी द्वारा ही बाहर आता है। अतः आपका जीवन बहुत अधिक वस्तुओं के कारण उलझनों से भरा नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक वस्तुओं तथा बहुत अधिक इच्छाओं के कारण आधुनिक जीवन में सादगी नहीं रह गयी है। धार्मिक मनुष्य सदैव गाता है, नाचता है। वह अपेक्षाकृत अधिक चिन्ता-मुक्त होता है तथा सादगी एवं सन्तोष-जनित आनन्द से भरपूर रहता है। हमें उससे ईर्ष्या होती है और हम सब-कुछ छोड़ कर उसका अनुकरण करने की चेष्टा करने लगते हैं-कम-से-कम कुछ समय के लिए तो अवश्य ही। आधुनिक मानव अनिच्छापूर्वक ही अपने जीवन को इतनी उलझनों से भरने देता है। वह जानता है कि सादगी ही सुख का रहस्य है। लेकिन 'यह मेरे वश की बात नहीं है' कह कर वह रुदन करने लगता है, नींद की गोलियाँ लेता है, मदिरालय जाता है। इस वर्तमान अपूर्णता को पूरी तरह भूलने के लिए वह कुछ करता ही है, जो कुछ भी सम्भव है, करता है।
सन्तोष रखिए। आप चाहे जैसी अवस्था में हों, उससे सुख ग्रहण करने की क्षमता रखिए और कहिए- "इस परिस्थिति में मेरे अनुभव को बदलने की शक्ति नहीं है। मेरा अनुभव उसी सीमा तक बदलेगा जिस सीमा तक मैं उसे अनुमति दूँगा। यदि मैं कहता हूँ 'नहीं', तो परिस्थिति कितनी भी परिवर्तित हो जाये, मुझमें वही शान्ति और सुख रह सकता है। परिस्थिति चाहे हर समय परिवर्तित होती रहे, मैं परिवर्तन-रहित रहूँगा।" अतः सादगी और सन्तोष से रहने पर सौभाग्य का द्वार आपके लिए खुल जायेगा। यहाँ तक कि आपको लगेगा कि आप हर प्रकार से उऋण हो गये हैं। हर दिन, हर महीने और हर वर्ष दी जाने वाली किश्तों का भूत जो सिर पर सवार था, हवा हो गया। कुछ लोगों को किसी भी तरह मुक्ति नहीं मिलती। जिनकी उन्हें किश्तें चुकानी रहती हैं, उन विभिन्न कम्पनियों के वे एक प्रकार से दास की तरह होते हैं। मृत्यु पर्यन्त उन्हें घर की, मोटरकार की, रेडियो या टी.वी. हो तो टी.वी. की, रेफ्रीजरेटर की, कपड़े धोने की मशीन की और इसी प्रकार अनेकानेक वस्तुओं की किश्तें चुकाते हुए बीतता है। भगवान् जाने कितनी त्रासदायक वस्तुओं का आविष्कार हो गया है !
सादा और सन्तुष्ट जीवन मानव-निर्मित वस्तुओं पर उतना निर्भर नहीं करता जितना ईश्वर द्वारा निर्मित वस्तुओं पर। यदि आपके पास देखने वाली आखें हों, तो सैकड़ों वस्तुएँ ऐसी हैं जो आपको आनन्द से भर सकती हैं। प्रातःकाल जब आप जागते हैं, तो कक्ष से बाहर आइए और ऊषाकाल को देख कर प्रसन्न हो जाइए। सूर्य को उगता हुआ देख कर और प्रसन्न होइए। चिड़ियों का चहकना आपको और भी आनन्दित करेगा। शीतल समीर भी प्रसन्नता का कारण होगा। इस प्रकार आपकी प्रसन्नता का अन्त नहीं रहेगा। केवल इन साधारण-सी प्रतीत होने वाली वस्तुओं यथा ऊषाकाल, सूर्योदय, पक्षियों का कलरव, बालकों की खिलखिलाहट, नीलाकाश, आकाश में विशाल जलपोत-सा विचरण करते हुए श्वेत मेघ, झूमते हुए छोटे-छोटे पुष्प आदि से सुख और आनन्द पाने की तकनीक सीख लीजिए। यदि आप यह जान लेंगे कि उनसे आनन्द कैसे प्राप्त किया जाता है, तो वे आपमें प्रेरणा भी भरेंगे। इस रहस्य को जान लेने पर आपके आनन्द का पारावार नहीं रहेगा।
दूसरों के सुख से भी आनन्दित होना सीखो। जब किसी को सुखी देखो तो इंष्यां करने की अपेक्षा प्रसन्न हो जाओ। दूसरों को सुखी देख कर आप भी सुखी हो जायें। दूसरों को सुखी बना कर उनके सुख में सुखी होना सीखो। दूसरों को आनन्दित कर आनन्द मनाने की तकनीक सीखो। आपका सुख सहस्र गुणा हो जायेगा। इस समय वह केवल आपकी अनुभूति में ही सीमित है; परन्तु यदि आप दूसरों से भी आनन्द पाने लगेंगे तो आप सतत सुखी रहेंगे, सबका सुख आपके सुख का एक अंग बन जायेगा तथा उसे अनेक गुणा बढ़ाता जायेगा।
केवल अपनी ही वस्तुओं के सौन्दर्य से ही नहीं वरन् सब पदार्थों के सौन्दर्य से आनन्द ग्रहण करने का यत्न करो। इस प्रकार आपमें सौन्दर्य-ग्रहण की निरपेक्ष क्षमता का विकास होगा। अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च किये बिना आप देखेंगे कि आनन्द का अक्षय कोश आपके चतुर्दिक्, आपके सब ओर बिखरा हुआ है। जब हम अनुभव करते हैं कि ईश्वर ने हमें सुखदायक कितनी-कितनी वस्तुएँ प्रदान की हैं, तो दिन-भर यदि उसका कृतज्ञता-ज्ञापन करते रहें, तब भी अधिक नहीं है। उसने हमें अकूत कोश दिया है।
अपने शरीर पर ही ध्यान दीजिए। आपके दो स्वस्थ नेत्र हैं। मान लीजिए, कोई कहता है-"अच्छा, अपनी एक आँख आप मुझे दे दीजिए। उसके बदले में मैं आपको एक लाख रुपया दूँगा।" स्वस्थ मस्तिष्क वाला कोई भी व्यक्ति क्या इस प्रस्ताव को मानने के लिए प्रस्तुत होगा? मान लीजिए, आपको ही आपकी जिह्वा के बदले एक लाख रुपये दिये जाते हैं, तो क्या आप देने को तैयार होंगे? इसका आशय है कि आपके पास लाखों-करोड़ों कीमत की वस्तुएँ हैं, परन्तु फिर भी यदि कुछ थोड़ी-सी चीजें हमारे पास नहीं हैं, तो उनके लिए हम जमीन-आसमान एक करते रहते हैं। उस समय हमें इसका ध्यान बिलकुल नहीं रहता कि हमारे पास तो पहले से ही अकथनीय मूल्य की वस्तुएँ हैं। कुछ अभागे जन ऐसे भी होते हैं जो इन अमूल्य वस्तुओं से वंचित रहते हैं। यदि आप किंचित् मात्र भी विचार करें कि ईश्वर ने आपको कितना अधिक दिया हुआ है, तो आपकी जीवन-दृष्टि ही बदल जायेगी।
इन छोटे रहस्यों को जानिए। ये साधारण हैं; परन्तु 'नावक के तीर' की भाँति अत्यधिक महत्त्व के हैं-अन्धकार के लिए जितना महत्त्व प्रकाश का है उतने ही महत्त्वपूर्ण!
जीवन के माध्यम से जो अनुभव आता है, उसे स्वीकारना सीखिए। उनके कारण रो-झींक कर अपने को दुःखी न कीजिए। ये अनुभव जितना दुःख लाते हैं, आप उनमें सम्भवतः और वृद्धि ही कर देते हैं। शान्त और विवेकशील रहिए। एक जो परम सत्ता है परा-बुद्धि, यहाँ का यह मानव जीवन उसी से निर्देशित होता है और ये अनुभव उसी स्रोत से, परा-बुद्धि से आते हैं। अतः मनुष्य की तरह उन्हें स्वीकारना सीखिए। जीवन के माध्यम से जो विपत्तियाँ आती हैं, उन्हें झेलिए। यदि थोड़ा दुःख भी है, तो उसे झेलिए और उसके डंक को निकाल फेंकना सीखिए। इस प्रकार जो अनुभव आपको कष्टदायक और अप्रिय लगते हैं, उनके द्वारा ही आप अपने जीवन को और समृद्ध बना सकते हैं।
सबसे मित्रता का व्यवहार करो। अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति विनम्रतापूर्ण शिष्टता रखं।। उनके समक्ष न भयभीत हों, न दब्बू और न ही घबराओ। इससे भी तुम्हारा आनन्द क्षीण हो जायेगा। प्रशान्त रहो। अपने समकक्षों के साथ मैत्री रखो। सबसे एकता का अनुभव करो। जो पद में, स्वास्थ्य में, बल में, सौन्दर्य में तुमसे घट कर हैं, उनके प्रति दयालुता, प्रेम और सहानुभूति का भाव रखो। जो दुष्ट हैं, दुःखदायी और पीड़क हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखो। स्वयं को खीज की, उत्तेजना की, क्रोध की अथवा अमित्रता और द्वेष की मनःस्थिति में न लाओ। उपेक्षा कर दो। ये चार प्रकार की अभिवृत्तियाँ यथा अपने से श्रेष्ठों के प्रति विनम्रतापूर्ण शिष्टता, समवयस्कों के प्रति मित्रता और भ्रातृत्व-भावना, अपने से नीचे के लोगों के प्रति दया और सहानुभूति तथा दुःखदायी दुष्टों के प्रति, आपसे द्वेष-भाव रखने वालों के प्रति पूर्ण उपेक्षा आपको ऐसे साधन प्रदान करेंगी कि आप सुखच्युत कभी भी नहीं होंगे। ये चारों मनोवृत्तियाँ आपमें होनी चाहिए।
सबसे बड़ी बात है कभी क्रोध के वशीभूत न हों। क्रोध ही ऐसा मनोभाव है जो अकेला ही सुख को नष्ट कर देता है। घर का पूर्ण सुख एक बार में ही पूर्ण रूप से विनष्ट कर डालता है। परिवार में यदि एक भी व्यक्ति तीव्र स्वभाव का है, तो वह अपने क्रोध से घर के अन्य सब व्यक्तियों का सुख तो नष्ट करता ही है, पड़ोसी भी उसके क्रोध का शिकार बन जाते हैं।
अपनी इन्द्रियों पर विवेकपूर्ण नियन्त्रण रखो। भौतिक सुख की, आनन्दोपभोग की इच्छा मानव-जीवन का एक स्वाभाविक अंग है; परन्तु यह केवल आपके मन और शरीर से ही सम्बन्धित है। इसी सन्दर्भ में हमें इन्हें जानना है। इतर जीवों की अपेक्षा श्रेष्ठ बुद्धि-युक्त होने के कारण, यह क्षमता मानव में ही है कि वह अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रख सकता है। इस प्रकार नियन्त्रण रखने से ये इन्द्रियाँ सुख को नष्ट नहीं कर सकती हैं। यदि आप इन्हें स्वयं पर हावी होने देंगे, उनके ऊपर लगे अनुशासन में ढील डाल देंगे, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। यह विश्व का विधान है।
अपने जीवन को धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और पवित्र बनाओ। यदि पवित्रता को आप अपने जीवन में पथ-प्रदर्शक बना लेंगे, तो आपके अन्तर से अपराध-ग्रन्थियाँ और स्नायविक उलझनें दूर हो जायेंगी और मनस् चिकित्सक की आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जो स्वयं को धर्मनिष्ठ बना लेते हैं, वे सुख से पूर्ण रहते हैं। जिस प्रकार सुख दिव्य गुण है, इसी प्रकार धर्म भी परम दिव्यता से ही निकला है। आरम्भ में चाहे यह कठिन हो; परन्तु यदि एक बार आप अपने जीवन को धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ बना लेते हैं, तो आप स्वयं को हर प्रकार के सिरदर्द से बचा लेंगे। आप एक झूठ बोलते हैं, तो उसका समर्थन करने में आपको अनेकानेक बार झूठ बोलना पड़ता है। सत्य से संलग्न होने पर आपकी समस्त परेशानियाँ और हजारों कण्टक दूर हो जायेंगे। सत्य और पवित्रता का जीवन उन कारणों से रहित होता है जो आधुनिक जगत में दुःख और कष्ट के हेतु हैं।
इससे भी अधिक आवश्यक है उस सर्व सुख, सर्व आनन्द और सर्व उल्लास के आन्तरिक महा-स्रोत की समीपता पाना। उसे आप चाहे जिस संज्ञा से, नाम से अभिहित करें, मैं उसे कोई नाम नहीं दूँगा। उसे अपनी सत्ता का केन्द्र बना लीजिए। वही शाश्वत तत्त्व है जो आपके जीवन को आधार देता है। वही आपका आद्यन्त है। वही आपका सब-कुछ है। आधार, गन्तव्य, ध्येय सब वही है। प्रेम बढ़ा कर उसी के निकट रहिए। उस परम से प्रेम कीजिए। सदैव स्मरण कीजिए।
जो ब्रह्मानन्द की अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, उन सिद्ध महापुरुषों ने सुख प्राप्त करने का एक अचूक रहस्य बताया है और वह रहस्य है भगवन्नाम। उन्होंने भगवन्नाम का अभ्यास करने को कहा है। वे कहते - ''नाम और नामी दो नहीं हैं। भगवान् का नाम और भगवान् एक ही हैं। यदि आपके अन्तर में परमात्मा का नाम है, तो परमात्मा भी आपके अन्तर में है।" यह महान् आध्यात्मिक सत्य है। यदि आप इस बात को स्मरण रखते हैं और दिव्य नाम को अपना बना लेने का यत्न करते हैं, सदैव दिव्य नाम का जप करते हैं, उसका आह्वान करते हैं और दिव्य नाम के प्रवाह से निरन्तर आपूरित हैं तो आप धन्य हैं, भाग्यशाली हैं।
सच्चे अर्थ में कहा जाये तो सुख आपके ही अन्तर में निहित अपरिवर्तनशील अनुभव है। यह वह चेतना है जिसके कारण आप शेष दूसरों से मधुरता ग्रहण करते हैं तथा जिसके अभाव में आप किसी भी वस्तु की किसी भी प्रकार की मधुरता ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। यह अत्यावश्यक तथ्य है।
अंकगणित में १ संख्या जिस प्रकार कार्य करती है, यह चेतना भी उसी प्रकार कार्यशील रहती है। यदि १ संख्या विद्यमान है, तो आप शून्य लगाते जाइए। प्रत्येक शून्य (०) के लगाने से उस संख्या का मूल्य अनुपातानुसार बढ़ता ही जाता है और इस प्रकार शून्य का बहुत ही अधिक महत्त्व हो जाता है। यदि संख्या १ वहाँ नहीं है, तो समस्त शून्य बिना किसी मूल्य के मात्र सिफर रह जाते हैं। इसी प्रकार केवल इस एक सत्ता की उपस्थिति से ही प्रत्येक पदार्थ में सुख देने की क्षमता पैदा हो जाती है। अतः इसे अपने जीवन का केन्द्र बनाइए। इसे अपने जीवन में सर्वोपरि महत्त्व का स्थान दीजिए। तब आप एक क्षण के लिए भी सुख से वंचित नहीं हो सकेंगे। उस सुख से आपको कोई भी दूर नहीं कर सकेगा; क्योंकि आप स्वयं ही वह सुख हैं। जब एक मछली को छोटे कटोरे से निकाल कर सागर में डाल कर मुक्त कर दिया जाता है, तो वह सागर में रहते हुए तैर कर कहीं भी जा सकती है। अतः इस भ्रान्त जीवन के छोटे से कटोरे से निकल कर हम महान् विशाल सत्य में प्रविष्ट हों। सुख ईश्वर में ही है और वह मेरे अन्तर में है तथा वह और मैं एक हैं।
नित्य सुख का अक्षय स्रोत अन्तर में विद्यमान है। ईश्वर करे, आप इस सत्य में जीयें। यदि ऐसा हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीवन सुख का प्रवाह हो जायेगा और इस प्रकार आपका जीवन अश्रुधारा की तरह न बह कर असीम आनन्द का अविराम प्रवाह बन जायेगा । मेरी प्रार्थना यही है । ईश्वर आपको सादगी और सन्तोष में, दीप्त गुणों में, विरक्ति की अवस्थ में, समस्त जीवों से मैत्री में पुष्पित होने की शक्ति और प्रेरणा दे । आपका जीवन आनन्द और उल्लास से पूर्ण हो । आनन्द, परमानन्द आपको प्राप्त हो।
१४. आध्यात्मिक साधना
हमारे अन्दर नित्य भगवान् की सर्वव्यापकता कीगहरी अनुभूति होनी चाहिए । वह नित्य विद्यमान आत्मा,परमात्मा हमारे कर्मोकोअध्यात्म की सुवास से सुवासित से सुवासित कर दे । चाहे हमारे कर्म सांसारिक हो, नीरस हों, गद्यात्मक हों, परन्तु हम सदा भगवान् की उपस्थिति की भावना करें, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं । अपनी सांसरिक दैनिक चर्या में आप जो भी कार्य करें, उसमें भगवान का दर्शन करें । यदि हम उसकी विद्यमानता की ऐसी शन्तिपूर्ण, आनन्दपूर्ण अनुभूति के साथ कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं और यही आज की परमावश्यकता है ।
'हम जो-कुछ भी करते है, वह सब समस्त नाम और रूपों मेंदृश्यमान उस नित्य शाश्वत ब्रह्म के प्रति हमारा समर्पण और पूजा है'- यह सम्यक भाव होना चाहिए । 'जड़-जंगम सब वही परमात्मा है'- समस्त कर्म इसी भावना से होने चाहिए ।
गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महराज के जीवन में यह भाव अद्भुत ढंग से चरितार्थ हुआ था । वे सभी में, जो उनके निकट आते थे, ईश्वर का अंश देखते थे । इसी भाव से वे गरीबों और बीमारों की सेवा करते थे । जीवन के अन्तिम क्षणों तक वे इसी भाव में रत रहे ।
परन्तु हमरे मन में कभी यह भाव आता भी है, तो हमारा कार्य मन को बहिर्मुखी बना देता है और भाव तभी आ सकता है, जब मन की वृत्ति अन्तर्मुखी हो। मन जब बहिर्मुख होता है, तो वह तुरन्त इन्द्रिय-विषयों से संयोग करता है । तत्परिणमत: मन पर प्रत्येक इन्द्रिय-विषय का अनिवार्यत: प्रभाव पड़ता है और यह भाव शिथिल पड़ जाता है । साथ-ही-साथ अन्य संवेग उदित हो जाते हैं। इसका उपचार क्या हैं? उपचार है केवल तीव्र अभिकांक्षा, सरलता और धैर्यपूर्ण अथक अभ्यास।
मन जब कभी भी बहिर्मुख हो, आप उसके एक अंश को केन्द्र से उसी प्रकार बाँधे रखिए जिस प्रकार जलपोत पर लगे ध्रुवदर्शक यन्त्र की सुई। जलपोत किसी भी दिशा की ओर क्यों न जाये, सुई सदैव उत्तर की ओर ही रहती है। इसके द्वारा मन का अन्तर-प्रवाह केन्द्रीय मूल-भाव को पकड़े रहेगा। यह स्थिति धीरे-धीरे अभ्यास द्वारा अर्जित कीजिए। इसके उपरान्त कोई भी उपाधि यदि मन को अस्थिर करना चाहेगी, तो भी इसे केन्द्रीय भाव से विलग नहीं कर सकेगी। एक अवस्था ऐसी भी आ जायेगी, जब यह भाव सम्पूर्ण रूप से कभी भी खण्डित नहीं किया जा सकेगा और हमारा जीवन सामान्य जीवन यापन का न रह कर भगवान् की सच्ची पूजा, साधना, तपश्चर्या और सही अर्थ में योग में बदल जायेगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है।
व्यक्ति के जीवन में इस भाव को अक्षुण्ण बनाये रखने और उसे तीव्र करने केलिए कतिपय व्यावहारिक निर्देश दिये जा रहे हैं। प्रातःकाल निद्रा त्याग द्वारा हम दिवस आरम्भ करते हैं और रात्रि में निद्रा में जाने के समय उसका अन्त करते हैं। अतः निद्रा त्याग कर जब हम प्रातः उठते हैं, तो मन में प्रार्थना का भाव होना चाहिए- 'भगवन्! समस्त नाम और रूपों में तुम्हारी पूजा करने उठा हूँ।" प्रातःकाल उठते ही ताजगी से भरे अपने मन में यह भाव लाइए कि आप विश्वरूपी भगवान् के पुजारी हैं। प्रार्थना कुछ इस प्रकार की हो- "भगवन्! आज दिन-भर मनसा वाचा-कर्मणा मैं जो कुछ भी करूँ, सतत तुम्हारी पूजा-रूप हो।" इस भावना के साथ कार्य आरम्भ करो। यदि आप इस भावना के साथ दैनिक चर्या आरम्भ करेंगे, तब आपको कर्म बाँध नहीं सकेंगे। आपके स्थान पर वे भगवान् के बँधने के कारण बन जायेंगे।
अपने दैनिक कार्यक्रम के मध्य में क्षणेक रुक कर अपने हो जाइए और कहिए- "यह जो-कुछ मैं कर रहा हूँ, सब भगवान् की पूजा है।"
समस्त जीवों में भगवान् को देखने की चेष्टा करें। बहुधा अपने को स्मरण कराते रहिए- "सर्वं ब्रह्ममयम्।" और अन्त में दिवस की समाप्ति पर शयन के लिए जाते हुए दिन-भर किये गये कर्मों को भगवान् के चरणों में यह कहते हुए अर्पित कर दें- "भगवन्! मैं तेरा हूँ, यह सब भी तेरा ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।" समझिए कि आप निमित्त हैं और भगवान् ही आपके मन, शरीर एवं इन्द्रियों द्वारा कर्मरत है। अपने समस्त कर्म और कर्मफल उसे ही अर्पित कर दें। आत्मार्पण की यही विधि है।
निमित्त बन जाइए। भावना कीजिए कि आपका निवास-स्थान भगवान् का मन्दिर है, आपके कर्म भगवान् की सेवा हैं, आपके द्वारा जलाया हुआ दीप उसकी आरती है और आप द्वारा उच्चारित प्रत्येक शब्द उसके नाम का जप है। आप जहाँ-कहीं जायें, उसकी उपस्थिति का अनुभव कीजिए। वह आपमें है, आपकी हृदय-गुहा में है। वह आपके मित्रों और हितैषियों से भी आपके अधिक निकट है। सबमें उसका दर्शन कीजिए।
सोने जाने से पूर्व भगवान् की प्रार्थना करने की आदत डाल दीजिए। प्रार्थना कीजिए- "मैंने हाथ, पाँव, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और मन से जो-कुछ भी किया, वह सब तुम्हारी पूजा-रूप में तुम्हें अर्पित करता हूँ।" और इसी विचार को मन में रखे सो जाइए। आध्यात्मिकता में यह भाव आपका सहायक होगा। यही आपके जीवन को व्यावहारिक आध्यात्मिकता प्रदान करता है। इतनी ही नहीं बल्कि दिन में जब कभी भी आप कोई विशेष कार्य करते हैं, प्रत्येक क्रिया के आरम्भ और अन्त में इसी को दोहराइए। उदाहरणार्थ भोजन के लिए बैठते समय भी आप सब पदार्थ भगवान् को अर्पित करें और तब भोजन आरम्भ करें। भोजन करने के उपरान्त भी 'ब्रह्मार्पणम्' कह कर उठें। पत्र लिखते समय भी इस मानसिक प्रार्थना के साथ बैठें- "भगवन्! यह भी तुम्हारी पूजा बन जाये।" और पत्र पूर्ण करने पर कहिए- "ब्रह्मार्पणम् !” हर एक समूचा कार्य जो भी आप आरम्भ करें, भगवान् की प्रार्थना से करें और समाप्ति पर उसे भगवान् को अर्पित कर दें।
दिन-भर के क्रियाकलापों को पूजा और यज्ञ में रूपान्तरित करने का यह बड़ा सरल-सा रहस्य और अत्यधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली तरीका है। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने ही इसका भी अन्वेषण किया था जिसे उन्होंने अमूल्य थाती के रूप में हमें प्रदान किया है। गीता में भी कुछ बड़े सुन्दर श्लोक हैं जिन्हें साधकों को निरन्तर स्मरण रखना चाहिए। यथा-
ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।। (गीता : ४-२४)
-अर्पण (आहुति-दान) ब्रह्म है; हवि (घृत) ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप अप्नि में ब्रह्मरूप होता जो होम करता है, वह भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी कर्म में ब्रह्मबुद्धि है, वह ब्रह्मभाव में निमज्जित हो ब्रह्म को ही उपलब्ध होता है। यह सर्वश्रेष्ठ प्रतिफल है जो मनसा-वाचा-कर्मणा शुद्ध भाव होने के कारण प्राप्त होता है।
१५. दिव्यता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है; अतः नियमित साधना द्वारा उसे प्रस्फुटित करो
आध्यात्मिक प्रस्फुटन का आशय आपकी चेतना का रूपान्तरण है। अतः आत्मिक प्रस्फुटन चेतना का रूपान्तरण है, जिसकी विभिन्न योगों के परिप्रेक्ष्य में भिन्न-भिन्न प्रकार से अर्थ-व्यंजना हो सकती है। सामान्य मानव जीवन में यह चेतना आखिर है क्या? हम स्वयं को अमुक व्यक्ति, अमुक की सन्तान और अमुक परिवार से, जाति से, घर-गृहस्थी से सम्बन्धित मानते हैं। 'मैं भारत का हूँ; वह अमरीका का है; मेरा इस व्यक्ति से, इस घर से, कार से, बँगले से, आफिस से सम्बन्ध है' आदि-आदि सोचते हैं।
अतः इस प्रकार हमारा चेतना-लोक बाहरी जगत् के अनेकानेक नातों-रिश्तों से भरा रहता है और ये सभी रिश्ते 'मैं अमुक हूँ', इस मूलभूत रिश्ते की अनुभूति से उद्भूत होते हैं। सबसे पहले 'यह मेरे पिता हैं, यह माता हैं, ये भाई-बहन हैं' आदि-आदि सम्बन्ध उगते हैं और इसके उपरान्त अन्य विविध सम्बन्ध आरम्भ हो जाते हैं। अतः हम चाहे जितना दर्शन बघारें, चाहे जितने ग्रन्थ पढ़ें, चाहे जितनी अध्यात्म-चर्चा करें, हमारी चेतना वही भौतिक स्तरीय चेतना मात्र ही रह जाती है, जिसका नाता हमारे इस भौतिक शरीर से तथा इसी तरह के अन्य स्थूल शरीरों और नाम-रूपों से है। अतएव यह चेतना पार्थिव (भू) चेतना, देह-चेतना और सांसारिक चेतना है। यदि आपकी चेतना पर पूर्णतः इस सांसारिक चेतना का आधिपत्य हो जाये, तो ब्रह्म-चेतना कैसे आ सकती है? उसके लिए कोई स्थान नहीं है। नेत्र बन्द करके यदि आप उसे अन्तर में लाना चाहें, तो चाहे वह आ जाये; परन्तु तुरन्त ही एक विजातीय वस्तु की तरह अन्तर्धान हो जायेगी।
एक महान् सन्त कहा करते थे- "यदि आप काई से आच्छादित किसी तालाब में कंकड़ डालें, तो क्षणार्ध काई उस स्थान से हट जायेगी; परन्तु तत्काल ही उसे पुनः आवृत कर लेगी। जल आपको दिखायी दे, उससे पहले ही वह काई से ढक जायेगा। जिस प्रकार यह काई तालाब के जल को पूर्णतः आच्छादित कर जल को दृष्टि से ओझल कर देती है और काई को हटाने का चाहे आप कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, वह बार-बार आ कर घनी हो जाती है। इसी तरह मानव की सहज चेतना भी जगत्-चेतना या भौतिक चेतना से पूर्णरूपेण ढकी रहती है।
समस्त मानवों की, यहाँ तक कि साधकों की भी यही तथाकथित सामान्य दशा है। परन्तु साधक निरन्तर ही इस जगत्-चेतना को दूर करने की प्रक्रिया का अनुगामी होता है। अतः सदैव ही कुछ उच्चतर चेतना उसकी चित्त-भूमि में क्रियाशील रहती है। परन्तु फिर भी यदि वह अपनी साधना के क्रम को कुछ क्षणों के लिए रोक दे, तो जगत्-चेतना (बोध) उस पर पुनः हावी हो जायेगी। आध्यात्मिक प्रक्रिया जगत्-चेतना को क्रमशः निःशेष करने और उसके स्थान पर अध्यात्म-चेतना को लाने का अविच्छिन्न, अनवरत और अशिथिल गम्भीर तन्मयतापूर्ण, सतत और अखण्डित प्रयत्न है। अध्यात्म-चेतना आ जाने पर आपको इस जगत् का, शरीर का तथा सांसारिक प्राणी के रूप में स्वयं का बोध न रह कर केवल उस ईश्वर का ही बोध रह जायेगा जो इन सबका कारण है तथा आत्यन्तिक सत्य है और अस्तित्व का भी सार-तत्त्व है। ब्रह्म-बोध प्रवेश करेगा, ब्रह्म-चेतना अन्तर में आयेगी और यह चेतना का रूपान्तरण अन्तःकरण की पूर्णरूपेण शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्रमशः आयेगा; क्योंकि चेतना स्वयं को मन के माध्यम से ही अभिव्यक्त करती है। और चेतना का वस्तुतः हमें कोई ज्ञान नहीं; क्योंकि हमने कभी भी अपनी सत्ता की गहराई को स्पर्श नहीं किया। वही (सत्ता) ही चेतना है।
हमारे लिए चेतना केवल एक संकल्पना या ख्याल मात्र है; अतः हम चेतना का बोध मानसिक चेतना या बोध को ही समझते हैं और बोध की हमारी यही परिभाषा है। परन्तु यह भावना और विचार-बोध मन के माध्यम से हुई अभिव्यंजना है। अतः सबसे पहले हमें मन के माध्यम से ही कार्य करना है। यदि हम मन के माध्यम से कार्य नहीं करते, तो इसके सिवा उस चेतना तक जो मनसातीत (Supramental) है, अति-मानसिक है, पहुँचने की और कोई विधि नहीं है।
आध्यात्मिक प्रक्रिया मन को समस्त पार्थिव सम्बन्धों से, समस्त स्थूल सम्बन्धों से, हर वस्तु से जो सांसारिक हो, जो राजसिक और तामसिक हो, असम्पन करने की प्रक्रिया है। आप इसे किस प्रकार करेंगे? ये तो कोई स्पर्ध्य या दृश्य वस्तुएँ नहीं हैं जो आप उन्हें एक-एक करके पकड़ें और बाहर कर दें। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तो मन के भीतर हैं, आन्तरिक हैं, साथ ही दिखायी पड़ने वाली नहीं है, अपूर्व हैं। साधक के सामने यही समस्या है।
ये सब ऐसे विचार, संवेग, अन्तःकरण की वृत्तियाँ, संस्कार, स्मृति, वासना, लालसा आदि हैं जो पूर्व-अनुभवों के कारण क्रमशः निर्मित हुए हैं। अतः सशरीर उनके पास पहुँच कर उन्हें निकाल फेंकने जैसी कोई विधि हम नहीं जानते। हम झाडू ले कर मन को निर्मल नहीं बना सकते। तब क्या किया जाये? केवल एक ही उपाय है और वह है मन में नवीन प्रतिपक्ष भावना और प्रतिपक्ष विचार सृजित किये जायें। वे धीरे-धीरे सबल होंगे, दृढ़ होंगे तथा अन्ततः बढ़ कर व्यापक होंगे और मन की वृत्ति में ही आमूल-चूल परिवर्तन कर देंगे; मन की वृत्ति में, उसकी सामान्य अवस्था में, उसके व्यवहार और कार्य के तरीकों में एक विपर्यय, एक परावर्तन ले आयेंगे।
इसकी उपलब्धि के लिए अनेक प्रक्रियाएँ बतायी गयी हैं। वे सब मिल कर ही साधना, आध्यात्मिक साधना कही जाती हैं। अतः प्रथम बात है चेतना का रूपान्तरण। आप संसार के प्रति या अपने शरीर के किसी अंग के प्रति जागरूक न रह कर स्वयं अपने प्रति जागरूक रहें। आप देह-चेतना में बँधे हैं तथा संसार के साथ आपका सम्बन्ध इसी देह-चेतना द्वारा सृजित होता है। यही कारण है कि देह-चेतना को छोड़ कर दिव्य चेतना को लाना है। आप ईश्वर के प्रति जागरूक रहें, शरीर या स्वयं के प्रति नहीं। आप स्वयं को प्रकाश-पुंज ईश्वर की एक ज्योतिर्मय किरण समझें, उसी प्रकार जैसे समुद्र और समुद्र की बूँद है। उसी प्रकार महासागर सच्चिदानन्द से, परम दिव्य से अनन्य समझें। आप असीम हैं, अनन्त हैं, अपरिमित हैं-ऐसी भावना करें। स्वयं को उसी का एक अंश समझें।
मन का केवल एक की कार्य हो-उस परम चैतन्य का चिन्तन। अतः साधना शुद्धिकरण की, एकाग्रता की, तादात्म्यता की और लीन होने की प्रक्रिया है। आपको चित्तशुद्धि करके दैवी चेतना के प्राथमिक तत्त्वों को जगाना होगा और उसे जगा कर आप केवल परम चेतना पर ध्यान एकाग्र करें, इस अवस्था को और सघन करें और अन्ततः उसी में लीन हो जायें। आप ज्यों-ज्यों साधना-पथ पर आगे बढ़ेंगे, ये अनुभव आपमें स्वतः आते जायेंगे। तत्त्वतः आप अमर आत्मा हैं जिसका न जन्म है न मरण, न दुःख है न बन्धन-नित्य शुद्ध और पूर्ण। यह भी आपमें पहले से ही है।
वेदों ने इसकी घोषणा की है। आपके गुरु ने भी आपको बताया होगा। उन्होंने कुछ ऐसे आकर्षक और हृदयग्राही तरीके से बताया होगा कि आपमें भी दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया होगा। अतः आप जानते हैं कि आप यह शरीर नहीं हैं, कि आप नित्य शुद्ध, पूर्ण तथा आनन्दमय आत्मा हैं। वह ज्ञान यहीं है, सम्भावना के रूप में। वह अनुभव के रूप में आपको प्राप्त नहीं है। आपको वास्तविक अनुभव नहीं है। आप समझते हैं कि आप अपने स्वरूप को जानते हैं; परन्तु चूँकि आपको आत्मानुभव नहीं हुआ है; अतः आप अज्ञानावस्था में हैं। इसीलिए यदि कोई आपको अपशब्द कहता है, तो आप तुरन्त स्वयं को अपमानित अनुभव कर उत्तेजित हो उठते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, बदला लेने के लिए, प्रतिशोध के लिए तत्पर हो जाते हैं। किसी के द्वारा सम्मान नहीं मिलता, तो आप तुरन्त अप्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी-सी भी हानि होने पर आप रोने-चीखने लगते हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अथवा कक्षा में प्रोन्नति न पाने पर या वेतन-वृद्धि न होने पर आप दीर्घ काल तक दुःखी रहते हैं। इस प्रकार आपको निरन्तर प्रत्येक घटना प्रभावित करती है और इन सबका प्रभाव पड़ने के कारण आप नहीं जान पाते कि आप नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध, नित्य पूर्ण और नित्य परिपूर्ण आत्मा है।
आपने चाहे आत्मानुभव प्राप्त न किया हो, केवल इतना जानना भर ही कि आप महामहिम सर्व ज्योतिर्मय आत्मा हैं, आपकी सहायता करेगा। इस ज्ञान का आंशिक कण भी बहुधा आपको आन्दोलित किया करेगा और आप सोचेंगे कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए; मैंने क्यों क्रोध किया? आत्मा तो किसी से भी प्रभावित नहीं होती, तो मैं ही क्रोध से अभिभूत कैसे हो गया?
आप प्रभु के हैं-ऐसा सोचिए। ईश्वर में कोई सृष्टि नहीं। दुःख आपको स्पर्श नहीं कर सकता। वहाँ बन्धन नहीं है, भय नहीं है। जब ईश्वर ही सब-कुछ है, तब आपको कुछ भी कमी नहीं है। अनुभव कीजिए कि आप ईश्वर की सन्तान हैं, आप उसी के हैं, वही आपके माता-पिता और सब कुछ हैं। आप यहाँ उसकी दिव्य महिमा के समभागी हैं। अनुभव एक चीज है; सम्भव ज्ञान दूसरी चीज है। सम्भव ज्ञान को विशेष प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में उतारना होगा, अनुभव में रूपान्तरित करना होगा। यह प्रक्रिया उस नित्य शुद्ध, निरंजन, निष्काम, दिव्य सत्ता का केवल ज्ञान ही नहीं देती प्रत्युत उस ओर गतिशील भी है। यह समस्त प्रक्रिया परम भाव, परम पूर्णता, सर्व गुण सम्पन्नता की अवस्था की ओर क्रमिक रूप में गतिशील है।
आध्यात्मिक आरोहण अथवा आध्यात्मिक विकास दैवी सम्पदा के अनुभव की ओर गतिशील प्रक्रिया है। इसका आशय है आरम्भ से ही समस्त साधना दिव्यीकृत होने की क्रमिक प्रक्रिया है अर्थात् हमारे जीवन में उन तत्त्वों के समावेश की प्रक्रिया है जो दिव्य कहे जाते हैं। समस्त साधनाओं की नींव यही है। यही वेदान्त, योग, भक्ति तथा कर्म-मार्ग की भी नींव है। यही हिन्दू, इसलाम, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा इसी प्रकार सभी धर्मों की नींव है। अतः आध्यात्मिक अन्वेषण की नींव, आधारशिला है क्रमशः असत् वस्तुओं का, समस्त अनुचित, अशुद्ध तथा आत्म-विचार से भिन्न विचारों का विनाश और दैवी सम्पदा (दैवी गुणों) का उत्तरोत्तर विकास जिससे हमारे अन्तस् में छिपी दिव्यता प्रकट हो सके।
निठल्ले मत बैठिए। आपका मूल-स्वरूप दिव्य है। यहाँ आप रोने-पछताने को नहीं आये हैं। अपने में अपने दिव्य स्वरूप का स्थापन करो। 'उत्तिष्ठत, जाग्रत' उठो, जागो। आप सत्य-पथ के पथिक हैं। आप दिव्य हैं। अपने शाश्वत आनन्द के धाम का मार्ग खोजिए। मानव होने का अर्थ है दुःखी होना। दैवी होना नित्यानन्द है। अपने हृदय में प्रभु की खोज को अपनी सर्वोपरि महत्त्वाकांक्षा बना लीजिए। मनसा-वाचा-कर्मणा इसी लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहिए।
आप अमुक हैं अथवा अमुक के पुत्र हैं, इस प्रकार से तादात्म्य करना सर्वथा छोड़ दीजिए। विशुद्ध सत्ता से, परम चैतन्य से तादात्म्य कीजिए। आप अमर हो जायेंगे। आप नित्यानन्द को उपलब्ध होंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त करें!
१६. मन : बन्धन और मोक्ष का कारण
आधुनिक मनोविज्ञान विधायक (Positive) सम्बन्ध का वचन देता है; परन्तु आत्मा को अछूता छोड़ देता है। आधुनिक मनोविज्ञान में आत्मा यों ही छूट जाती है; क्योंकि उसमें आत्मा की कोई संकल्पना नहीं है। उनका कहना है कि शरीर और चित्त-सत्ता (Psychic Being) घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है; परन्तु इस कथन से वेदान्तिक दृष्टिकोण बिलकुल ही प्रभावित नहीं होता। चाहे आप जानते भी हों कि दोनों अखण्ड रूप में जुड़े हैं; परन्तु इससे आत्मा का क्या सम्बन्ध ? क्योंकि आत्मा तो चित्त-सत्ता और सूक्ष्म सत्ता से भी भिन्न है। आत्मा मानव-व्यक्तित्व को बनाने वाली समस्त वस्तुओं से भिन्न है। अपने स्वरूप अर्थात् आत्मिक स्वरूप के अतिरिक्त वह सबसे भिन्न है और उसका स्वरूप शुद्धात्मा, शुद्ध सत्ता अनादि, अनन्त है जो परिवर्तनहीन और शुद्ध चेतन है। अतः उसे आप शुद्ध चैतन्य, चिन्मय और सच्चिदानन्द के रूप में जानिए।
क्या व्यक्तित्व (अहं) को खोये बिना आत्मा और शरीर में भेद दिखायी दे सकता है? वस्तुतः यह उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं; क्योंकि जैसा हम सामान्यतः सोचते हैं, वैसा ही यह शरीर और आत्मा की परस्पर भिन्नता नहीं है। यह तो आत्मा और अनात्मा का अन्तर है। शरीर ही नहीं प्रत्युत जो कुछ भी अनात्मा की परिभाषा में आ सकता है, उस सबसे भिन्नता है। यदि आपमें तपोबल है, तो आप समझ सकते हैं कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है?
आत्मा से इतर जो-कुछ है, उस सबको पतंजलि ऋषि ने 'प्रकृति' कहा है। अतः अपनी निर्विकल्प समाधि में आप जो अनुभव करते हैं, वह पुरुष और प्रकृति के अन्तर को अनुभव करते हैं। पुरुष आत्मा है और प्रकृति सब-कुछ जो अनात्म है, वह है। अतः शरीर, पंच-इन्द्रियाँ, पंच-कोश, अन्तःकरण (मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार), पंच-प्राण, समस्त वासनाएँ, संस्कार, सारी विश्व-प्रक्रिया, सारा जगत्-जंजाल आदि-आदि सब-कुछ प्रकृति में ही है और इस कारण प्रत्येक चित्त-वृत्ति या जो-कुछ भी इन्द्रियानुभव द्वारा निर्मित है वह सब, प्राण, मन यहाँ तक कि अहंकार भी तथा संस्कार, वासनाएँ, प्रवृत्तियाँ सभी कुछ प्रकृति में सम्मिलित हैं। याद आप एक बार भी इस अन्तर को जान जायेंगे, तो संसार की क्रियाएँ आपको कभी भी दुःखी नहीं कर सकेंगी।
पुरुष और प्रकृति में भेद है; परन्तु मन के रहते यह भेद ज्ञात नहीं हो सकता। परन्तु मनोनाश हेतु, अहं-शून्यता हेतु साधक को परेशान नहीं होना चाहिए; क्योंकि यह अहंता जो मिथ्या अहं ही है, इसकी स्वयं में कोई सत्ता नहीं होती। प्रकृति के सान्निध्य में आने से चेतना में जो उलझाव पैदा हो जाता है, वही मिथ्या व्यक्तित्व (अहं) का कारण है। जब प्रकृति के इस सान्निध्य को विच्छिन्न कर दिया जाता है, तो केवल वास्तविक सत्ता शेष रह जाती है। मिथ्या वस्तु का नष्ट हो जाना किसी वस्तु का नष्ट हो जाना नहीं कहा जा सकता। जब हम जान जाते हैं कि जीव-चेतना प्रकृति का ही अंश है, हमारी वास्तविक सत्ता नहीं है, तब उसका अभाव वस्तुतः कोई महत्त्व या अर्थ नहीं रखता। यही कारण है कि केवल मन का नियन्त्रण ही राजयोग का लक्ष्य नहीं है। आरम्भ की अवस्थाओं में मन का नियन्त्रण किया जाता है जिससे एकाग्र चित्त के नियमन द्वारा आगे चल कर एक ऐसी अवस्था की प्राप्ति की जाये जिसमें मन का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है।
राजयोग-दर्शन में कहा गया है कि निरोध से ही योग होता है। निरोध ध्यान की अवस्था प्राप्त करने हेतु कुछ ही दूर तक के लिए होता है, ध्यानावस्था में आने पर अति-चैतन्य में प्रवेश करने के समय चित्त और अहं की भूमिका को पूर्णरूपेण त्याग देते हैं। अति-चैतन्य की भूमिका पर मन का अस्तित्व नहीं रह जाता। इस भूमिका पर आप परम पुरुष का साक्षात्कार करते हैं, मन निःशेष हो जाता है। जब तक आप मन-सत्ताविहीन भूमिका पर नहीं पहुँच जाते, आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मानुभव के लिए मन-विहीन अवस्था अपरिहार्य है। अतः इस अवस्था को पहुँचने के लिए मन की वृत्तियों का पूर्ण नियन्त्रण और पूर्ण निरोध आवश्यक सोपान और आवश्यक अनुशासन होते हैं। राजयोग उसी अनुशासन को देता है और जब यह अनुशासन पूर्णता को पहुँच जाता है, आप मनसातीत हो जाते हैं, मन का अतिक्रमण कर जाते हैं। मनसातीत होने या अहं-शून्य होने पर साधक को चिन्तित नहीं होना चाहिए। यह अहन्ता अति-विनाशकारी होती है। यह चेतना की सबसे बड़ी व्याधि है, शुद्ध चेतना पर अशुद्धता का धब्बा है। अतः अहं को खोना महा-उपलब्धि है।
अब यहाँ एक शंका उदित होती है कि विकास के क्रम में मानव-स्तर पर ही जब उच्चतम विकास की अवस्था मानी गयी है, तो हम व्यक्तित्व के मूल तत्त्व को क्यों विनष्ट करें? आइए, देखें तो आप मानव-स्तर से क्यों चिपके रहना चाहते हैं? निस्सन्देह, यह स्तर मानवेतर जीवधारियों में एक-कोशीय जन्तु से ले कर अपृष्ठवंशी कृमि-कीट, मत्स्य, सरीसृप, पक्षी, पशु के क्रम तक तुलना करने पर सभी की अपेक्षा उच्च है। ठीक है, परन्तु आपको इसी स्तर से नहीं चिपके रहना है।
मान लीजिए, तीन-'अ', 'ब' तथा 'स'-श्रेणियों के कैदी हैं। 'स' श्रेणी वाले कैदियों को नित्य कोड़े लगते हैं, प्रतिदिन बारह घण्टे धूप में पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, भोजन में सूखी रोटी-पानी मिलता है और भूमि पर सोना पड़ता है। 'ब' श्रेणी के कैदी भोजन में अतिरिक्त सब्जी पाते हैं, मच्छर और फर्श पर रेंगने वाले जन्तुओं से शरीर-रक्षा हेतु सोने को चारपाई मिलती है और कदाचित् कार्य भी दस घण्टे ही करना पड़ता है। 'अ' श्रेणी के कैदियों को अच्छे कमरे दिये जाते हैं, भोजन आदि स्वयं बनाने की अनुमति भी होती है और श्रम-कार्य नहीं करना पड़ता। उन्हें समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ भी मिल सकते हैं। प्रायः धूम्रपान की सुविधा भी होती है। सप्ताह में एक दिन बाहर से मिलने वाले व्यक्तियों को भी जेल के अन्दर जा कर मिलने की अनुमति होती है। अतः क्या आप सोचेंगे कि अब चूँकि मैं 'अ' श्रेणी का कैदी बन गया हूँ, अतः कारागार से मुक्त होने की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार दूसरी अन्य अवस्थाओं की तुलना में मानवावस्था अधिक उन्नत है; परन्तु अभी भी यह बन्धन ही है।
आत्मा की मुक्ति कुछ इस प्रकार से अकल्पनीय रूप से भव्य और विशिष्ट है कि विकास की वर्तमान अवस्था भी उसके समक्ष बन्धन है। उसकी समता में यह नरक है; परन्तु इतर अन्य अवस्थाओं की तुलना में यह स्वर्ग है और ईश्वर-सृष्टि की शान है; क्योंकि मानव ईश्वर की अनुकृति है। लेकिन मनुष्य भी बड़ा अधम हो सकता है। वह ऐसे कार्य कर सकता है जो पशुओं को भी करते लज्जा आती हो तथा जो कभी-कभी पशु भी नहीं कर सकते। जिसे पशु भी नहीं कर सकते, उसे भी कभी-कभी मनुष्य कर बैठता है। मानव-जीवन की यही अपूर्णताएँ एवं त्रुटियाँ हैं अथवा यदि हम मान लें कि मानव-जीवन बड़ा सुन्दर है, बड़ा अच्छा है, सुखमय है, अद्भुत है, पूर्ण है तब भी उस स्थिति में इससे कौन चिपका रहना चाहेगा जब कि कोई अन्य अवस्था इससे भी शत गुणा उत्तम हो? दिव्यावस्था ऐसी ही है। जब इसकी अपेक्षा अधिक उत्तम, उच्च और श्रेष्ठ अवस्था भी है, तो इसी निम्न अवस्था में संलग्न रहने की इच्छा करना बुद्धिमानी नहीं है।
विचारणा-शक्ति ही मानव-जीवन का सार है तो मन को हम किस प्रकार निःशेष कर सकते हैं। डिस्कार्ट कहता है: "I think, therefore, I am" - "मैं विचार करता हूँ; अतः मैं हूँ" अथवा "मैं हूँ, इसीलिए मैं विचार करता हूँ।" हम हर एक वस्तु को नकार सकते हैं, हर एक वस्तु पर सन्देह कर सकते हैं; परन्तु सन्देहकर्ता पर सन्देह नहीं कर सकते। लेकिन डिस्कार्ट ने इतना ही कह कर छोड़ दिया है। यह 'मैं' कौन है जो कहता है-"मैं विचारता हूँ, अतः मैं हूँ?" और 'मैं' का असली स्वरूप क्या है? दर्शन की यही विषय-वस्तु है, यही प्रतिपाद्य है।
उपनिषदों में इस 'मैं' के स्वरूप का अति-सुन्दर वर्णन है। वे उपनिषद् आत्म- साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था के सहज उद्गार हैं तथा गहन ध्यान और सहज प्रज्ञा द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊँची उड़ान से उपलब्ध संसिद्धि की उद्घोषणाएँ हैं। उन्होंने अनुभव किया कि यह जीव, यह 'मैं' जो कहता है- 'मैं विचारता हूँ, अतः मैं हूँ' अतिमानसिक जीव-सत्ता है। मन से आगे है। यह मन का अतिक्रमण कर लेती है। यह उस वास्तविक 'मैं' को उपलब्ध कर लेती है जो मन से अतीत है, मन की पहुँच से बाहर है। इस तरह आपने देखा कि आपको इस चिन्तन-शक्ति से छुटकारा पाना है, क्योंकि यह आपके लिए एक अवरोध है। जब तक यह चिन्तन-शक्ति (विचार-शक्ति) मानव-जीवन का सार-तत्त्व रहेगी, तब तक मन को निर्मूल कैसे कर सकते हैं?
ठीक है, चिन्तन-शक्ति मानव जीवन का सार-तत्त्व तो है, परन्तु आपका सारभूत स्वरूप मानव-स्वरूप नहीं है। आप मानव-प्राणी नहीं हैं; अतः स्वयं को मानव-प्राणी समझने की भूल न करते रहिए। आप मानव नहीं हैं। आप दिव्य हैं। तत्त्वतः आप ईश्वर हैं। अतः आपको इस मानव-स्वभाव को तथा मानव-स्वरूप की सारभूत शक्ति इस चिन्तन-शक्ति को त्याग देना है। जब तक आप चिन्तन करते रहेंगे, तब तक आप मानव-लोक में ही आबद्ध रहेंगे। अतएव एक समय आता है जब मन बाधक बन जाता है। आरम्भ में मन साधन होता है, पथ होता है, सहायक होता है; परन्तु एक स्थिति आती है जब मन बाधक बन जाता है। और जब वह अवस्था आती है, तब मन की उपेक्षा कर देनी पड़ती है।
एक सुबोध दृष्टान्त दिया जा रहा है। मान लीजिए, आप ऊपर छत पर चढ़ना चाहते हैं। इस समय आप भूमि पर हैं और सीढ़ी आपकी सर्वश्रेष्ठ मित्र है। उसके बिना आप ऊपर नहीं जा सकते। सीढ़ी के एक-एक डण्डे पर चढ़ते जाइए। आप ऊपर अन्तिम डण्डे तक पहुँच जायेंगे। मान लीजिए, आपको उस सीढ़ी के प्रति ही आसक्ति उत्पन्न हो जाये और आप कहने लगें, 'ओह, इसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है।' और आप उस सीढ़ी को छोड़ना न चाहें, तब क्या होगा? आप छत पर नहीं पहुँच सकेंगे।
एक समय आता है जब आप सीढ़ी के अन्तिम सिरे पर पहुँच कर खड़े हैं और आपको निश्चय करना है-"सीढ़ी ने निस्सन्देह इस ऊँचाई तक पहुँचने में बहुत सहायता की है; परन्तु यदि अब भी मैं इस पर ही खड़ा रहूँ, तो छत पर पहुँचने के आनन्द से वंचित रह जाऊँगा। अतः यदि मुझे छत पर जाना है, तो सीढ़ी को छोड़ कर छत पर कूद जाना है।" अब तक इस ऊँचाई तक, जहाँ सीढ़ी और छत मिल जाते हैं, सीढ़ी अपरिहार्य थी, अत्यावश्यक और बहुत सहायक थी; परन्तु जब इस ऊँचाई पर आ गये हैं, तब सीढ़ी पर ही रुक जाना एक बड़ी बाधा है, एक बड़ी भूल है। अतः यदि आप छत पर पहुँचना चाहते हैं, तो सीढ़ी को त्याग देना पड़ेगा। आध्यात्मिक अनुभव के सन्दर्भ में मन की भी यही स्थिति है। उच्चतम अनुभव वह अवस्था है जहाँ मन बाधक बन जाता है, परन्तु उस स्तर तक पहुँचने में मन सर्वोपरि सहायक होता है, अपरिहार्य साधन बनता है।
१७. आध्यात्मिक विश्व-गुरु स्वामी शिवानन्द
हम प्रतिवर्ष पहली जून को अपने पूज्य गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का संन्यास-दीक्षा-दिवस मनाते हैं। इस महान् पुनीत अवसर पर आइए, हम श्री आचार्य शंकर तथा संन्यास की उनकी देदीप्यमान परम्परा का स्मरण करें जो इस महान् भूमि की, इस भारत की गरिमामयी आध्यात्मिक आलोक-रेखा रही है। उन सन्तों और महापुरुषों की सन्त-परम्परा को स्मरण करें जिन्होंने इस भूतल पर संन्यास की गौरवमयी परम्परा को अक्षुण्ण रखा। आज उस परमेश्वर के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करें जिसने हमें अनूठा अधिकार दिया है कि हम अपने को गुरु महाराज के शिष्य कह सकें तथा उनके व्यक्तिगत जीवन का निकट से विनम्र अवलोकन करके मानव-सत्ता का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकें।
मानवता के विशाल हृदयी हितैषियों का जीवन अपने हित और लाभ को, अपनी प्रिय से प्रिय लगने वाली वस्तुओं को जन-कल्याण के लिए निःसंकोच उत्सर्ग करता आया है। इस आधुनिक सन्त की भी ऐसी ही कथा है-तीव्र संवेदनशील हृदय, तुरन्त अचानक निर्णय ले लेने और त्याग की तत्परता की कथा - ऐसी तत्परता जो मानवता की सेवा और अभ्युत्थान हेतु पूर्णरूपेण समर्पित जीवन के रूप में विकसित हुई।
श्री स्वामी शिवानन्द जी का नाम सर्वत्र सहस्रों ऐसे व्यक्तियों को जाग्रत, प्रेरित और उद्बोधित करने वाले के रूप में जाना और माना जाता है जो कि यदि इस प्रकार उद्बुद्ध न किये गये होते, तो उच्चतर जीवन और महत्तर आदर्शों के विषय में उभरने वाले समस्त प्रश्नों के प्रति उदासीन ही बने रहते ।
वे ८ सितम्बर १८८७ को पैदा हुए थे। उनमें प्रारम्भ से ही रुग्ण व्यक्तियों की सेवा करने, दुःखियों के दुःख दूर करने तथा जरूरतमन्दों की सहायता करने की भावना बलवती थी। अतः अपने प्रतिभाशाली कालेज-जीवन के उपरान्त आपने डाक्टरी पढ़ी। २५ वर्ष की आयु में, १९१३ के प्रारम्भ में ही उन्होंने मलय प्रायद्वीप के एक अस्पताल में डाक्टरी करना आरम्भ कर दिया और दस अविस्मरणीय वर्षों तक यह युवा डाक्टर पूर्ण उत्साह के साथ अथक रूप में जनता के कष्ट, पीड़ा और बीमारियों को दूर करने के प्रयत्न में लगा रहा। परन्तु संन्यास-पथ पर चलने की आन्तर जीवन की आकांक्षा बढ़ती जा रही थी; अतः जीवन के उच्च और भव्यतर कर्तव्य का आह्वान उन्हें सांसारिकता से निकाल कर विशुद्ध जीवन की आध्यात्मिक भूमिका पर ले आया। इस प्रकार सन् १९२३ ने उन्हें भारतीय आकाश के नीचे हिमालय की ओर एकाकी, अकिंचन, निष्काम जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध जिज्ञासु के रूप में बढ़ते देखा। निश्चय ही वह दिन वास्तव में अत्यन्त शुभ दिन था।
सन् १९२४ में उन्होंने ऋषिकेश में संन्यास-दीक्षा ली और तुरन्त ही कुछ काल के लिए अपनी ही चलायी हुई 'सत्य सेवा आश्रम डिस्पेंसरी' के माध्यम से निष्काम सेवा में जुट गये। लगभग डेढ़ वर्ष के उपरान्त वे एकान्त और ध्यान में लग गये। सन् १९३५ तक उनका जीवन कठोर तपश्चर्या, ध्यान, आन्तर साधना और ज्ञानोपलब्धि का जीवन था। परन्तु वे तो कर्तव्यारूढ़ थे। अतः आत्महन्ता भौतिकता के पाश में जकड़ी मानवता की अनवरत पुकार उन्हें ध्यान और चिन्तन के क्षेत्र से बाहर निकाल कर विश्व-सेवा के उदात्त क्षेत्र में ले आयी।
अध्यात्म-ज्ञान के प्रसार का उनका उद्देश्य उन्हीं के द्वारा सन् १९३६ में द डिवाइन लाइफ सोसायटी' (दिव्य जीवन संघ) की स्थापना के द्वारा कार्यान्वित हुआ। सन्देहवाद, अधर्म और इन्द्रियलोलुपता के आधुनिक रोग का कारण तथा उसके उपचार के विषय में निरन्तर विचार करते-करते स्वामी जी की गहरी सहानुभूतिप्रवण प्रबुद्धता ने उस मूल कारण को खोज लिया जो चौड़ी होती हुई खाई के रूप में भूमिपुत्रों को उनकी जीवनदायिनी प्राचीन विद्या के दिव्य ज्ञान से अलग करना आरम्भ कर चुकी थी।
शासक-वर्ग द्वारा थोपी गयी शिक्षण पद्धति तथा शास्त्रों की प्राचीन शास्त्रीय भाषा-दोनों ही इसके प्रति उत्तरदायी हैं और स्वामी जी आध्यात्मिक जीवन के महान् सत्य को पूरे राष्ट्र में प्रसारित करते हुए इसी घातक अज्ञानता से जूझ रहे थे। उन्होंने शास्त्रों के सन्देश को, कथ्य को पश्चिमी सभ्यता में रंगी पीढ़ी के लिए, देश की भावी आशा के लिए सुलभ कर दिया।
यदि हम देखें कि प्राचीन युग के संन्यासियों की भाँति स्वामी जी भी आ कर गंगा जी के तट के निकट एक पुण्य स्थल पर जम कर रहने लगे थे, तो उनके इस कार्य का विस्तार आश्चर्य से किसी प्रकार भी कम नहीं था। उनका जागरण का यह सन्देश भूमण्डल की प्रत्येक दिशा में पहुँच कर युवा और वृद्ध सभी में नैतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान ले आया और इस प्रकार उनके परिश्रम का सुखद फल प्रकट हुआ। प्राणी मात्र में शिव का दर्शन करने से उनका प्रत्येक कर्म विश्वात्मा के प्रति पूजा और श्रद्धामय होता था।
वे आधुनिक पीढ़ी के अन्दर अपनी महान् सभ्यता और संस्कृति की महिमा का भाव जगाने और भारत माँ की अपनी परम्पराओं, संस्थाओं तथा प्रतिभाओं के प्रति स्वस्थ श्रद्धा और सम्मान की भावना उत्पन्न करने में सफल रहे। उनके वचनों और उनके कार्यों द्वारा साधारण मनुष्य भी समस्त मानवों में निहित एकत्व का अनुभव करने लगा है। श्री स्वामी जी निरन्तर यही सत्य हृदयंगम कराते रहे कि बाहरी भिन्नता और पृथकता और कुछ नहीं केवल व्यर्थ की चीज है; अतः महत्त्वहीन है। समस्त जीवों का तात्त्विक भाव तो आत्मिक है जो विश्व भर में सर्वत्र एक-सा है। इस प्रकार श्री स्वामी जी का आविर्भाव राष्ट्र और विश्व को एक करने वाली शक्ति के रूप में हुआ था।
भारत की नियति में आस्था रखते हुए, विश्व के आध्यात्मिक मार्गद्रष्टा के रूप में वे विश्व को उस महान् कर्तव्य के प्रति समग्र रूप से सजग करने में प्रयत्नशील रहे। इस तरह वे आबाल-वृद्ध, नर-नारी सभी में यह आत्मिक चेतना का भाव जाग्रत करने में लगे रहे। 'दिव्य जीवन संघ' की अनेकानेक शाखाएँ समूचे परिवारों के लिए अध्यात्म-शिक्षा तथा पुनरुत्थान के केन्द्र हैं। परिवार के बालकों, युवकों, माताओं और यहाँ तक कि सेवकों और प्रतिवेशियों को प्रेरणा और प्रशिक्षण देने की ये विलक्षण इकाइयाँ हैं। स्वामी शिवानन्द जी महाराज अकेले ही प्रभावशाली आध्यात्मिक प्रचार नहीं करते थे। उनमें एक विचित्रता थी कि जो उनके प्रतिभा-शक्ति-सम्पन्न व्यक्तित्व की सीमा में आया, उन सभी को उन्होंने अध्यात्म का उत्साही प्रचारक बना दिया।
वे प्रायः चुप रहते थे; परन्तु फिर भी विभिन्न वर्गों के लोगों के परस्पर विभेदों को दूर करने, उनके अवरोधों को हटाने तथा उनमें सौहार्द्र, सद्बुद्धि लाने की सशक्त, सक्रिय क्षमता से भरे थे। अपनी वरद लेखनी के अनवरत श्रम द्वारा, प्रेरणादायक पत्रों में व्यक्तिगत चेतावनी, निर्देश और सुझावों द्वारा तथा 'द डिवाइन लाइफ सोसायटी' की अनेकानेक शाखाओं के लिए मौन रूप में किये गये कार्यों द्वारा उन्होंने सहस्रों लोगों के अन्तर में नैतिक और आध्यात्मिक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। अतः यदि हर जाति, धर्म, मत या सम्प्रदाय के अगणित लोग एकमात्र उन्हें ही अपना पथ-प्रदर्शक और गुरु मानने लगे हों, तो कुछ आश्चर्य नहीं।
उनके अध्यात्म-ज्ञान-दान में सदा ताजगी रहती थी। वे केवल उद्बोधन और प्रेरणा दे कर ही नहीं रुक गये। उन्होंने हर स्तर के साधकों के लिए सुनिश्चित व्यावहारिक कार्यक्रम की रूपरेखा देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी और इस प्रकार साधकों को वे हर पग पर निर्देशन, सुझाव, उत्साह और ज्ञान देते चलते रहे।
वे अन्य मतवादियों की भाँति धार्मिक विश्वास के प्रति दुराग्रही नहीं थे। धर्म के प्रश्न के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टि रखते थे और जहाँ-कहीं आवश्यकता हुई, तो स्पष्ट अपरोक्ष रूप से आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे। धर्ममय जीवन और आध्यात्मिक पथ के पूर्ण रूप से पक्षधर होते हुए भी उन्होंने हर स्तर पर इस पथ में उपस्थित होने वाले गह्वरों और बुराइयों का भी उद्घाटन किया तथा इस पथ की त्रुटियों की ओर संकेत करते हुए इसका निन्दनीय प्रयोग करने की आलोचना की। उनकी इस विशेषता का सबसे बड़ा महत्त्व तो यह रहा है कि इससे कठोर साधन-पथ पर चलना आरम्भ करने वालों को पूर्णरूपेण चेतावनी मिलती रही है। पूर्व से ही प्राप्त उनकी स्पष्ट चेतावनी साधकों के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र के अदृश्य तत्त्वों से लड़ने के समय सुरक्षा की ढाल का काम करती है।
आज के संसार के युवा मनुष्य पर श्री स्वामी जी के उपदेशों का जो विलक्षण आकर्षक प्रभाव पड़ा है, वह दोहरे तत्त्वों से उद्भूत है, यथा उनका किसी भी मत-विशेष का अवलम्बी न होना तथा अनावश्यक, अस्पष्ट एवं जिनका कोई भी मूल्य नहीं ऐसे तथ्यों को नकार कर महत्त्वपूर्ण, वास्तविक तत्त्वों पर विवेकपूर्वक बल देते हुए व्यावहारिक धर्म का प्रस्तुतिकरण ।
कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी कथनी से नहीं, करनी से जाना जाता है। आनन्द कुटीर का यह सन्त उक्त कथन को पूर्णतः चरितार्थ करता है; क्योंकि सहस्रों ऐसे कृतज्ञ लोग हैं जिनका अविश्वास की अन्ध गहराइयों से उबरा हुआ जीवन श्रद्धा, भक्ति और सौभाग्य के शिखरों का स्पर्श कर रहा है।
उनके सरल, सबल और प्रमुख व्यावहारिक उपदेशों की प्रेरणा से स्त्री-पुरुष धर्म को अपने जीवन में एक विधेयात्मक, रचनात्मक, मुक्तिदायक शक्ति समझने लगे हैं जो उन्हें हताशा और दुर्बलता से हटा कर उनमें नवीन आशाएँ और आन्तरिक ओज भरती है।
विशुद्ध प्रेम के नाते, आध्यात्मिक दिशा में इस सारे श्रम को करते हुए भी वे उस शाश्वत केन्द्र से नित एक थे। चलते-फिरते, जीवन यापन करते उनकी सत्ता सतत रूप में उस परम सत्ता के प्रति सजग थी-केवल इसलिए कि इस व्यक्ति ने पार्थ-सारथि द्वारा बताये दिव्य संकेत को दृढ़तापूर्वक ग्रहण किया था :
“यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति-मुझे सबमें देखो और सबको मुझमें देखो।"
मेरी प्रभु से कामना है कि आप सब पर भी उनकी ऐसी ही कृपा हो!
१८. भागवत में भक्तियोग
अठारह पुराणों में श्रीमद्भागवतपुराण सर्वाधिक महत्त्व का है। इसीलिए यह महापुराण कहलाता है। इस पुराण में भगवान् विष्णु अर्थात् भगवान् नारायण की दिव्य महिमा का गान है। भगवान् विष्णु से हमारा सर्वोपरि सम्बन्ध है; क्योंकि इस जीवन के, जगत् के, इस विश्व-प्रक्रिया के, यहाँ तक कि जो कुछ भी यहाँ घटित होता है, उस सबके धारणकर्ता, पालनकर्ता एवं रक्षक वे ही हैं।
दिव्य शक्ति से जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, वह तीन मूल-रूपों में प्रकट होती है। उसके अनेकानेक रूप हैं; परन्तु हमारा सम्बन्ध उनके तीन मुख्य रूपों से ही है। कारण, हम विश्व में हैं और विश्व शुद्ध अव्यक्त परम सत्य की अवस्था से उस समय प्रकट हुआ जब यहाँ न कोई नाम-रूप था न सृष्टि, केवल परम सत्य अद्वैत था। आदि में ईश्वर था। केवल वही था और उसमें संकल्प हुआ-"प्रकटीकरण हो जाये, प्रकाश हो जाये।" सृष्टि-रचना के विषय में बाइबिल कहती है-"प्रकाश हो जाय।" उपनिषद् कहते हैं- "आदि में केवल वही था-अद्वितीय, परम, केवल१ और उसमें एक रहस् निगूढ़ भावना उदित हुई- 'मैं अनेक हो जाऊँ२ और दिव्य संकल्प मात्र से वह एक से अनेक हो गया।"
प्रकट होने की यह प्रक्रिया दिव्य शक्ति के कर्तृत्व-पक्ष द्वारा होती है। उसके इसी पक्ष को सृजन-शक्ति, सृष्टि को आकार देने वाली शक्ति भी कहते हैं। देवी के इस महासृजनशील पक्ष की कल्पना जब मनुष्य के रूप में अथवा मूर्त रूप में करते हैं, तब उसे 'ब्रह्मा' - सृष्टिकर्ता कहते हैं। कल्प के अन्त में यही शक्ति समस्त नाम-रूपों को पुनः उसी अव्यक्त में अदृश्य और लीन कर देती है, तो नाम-रूप-हीन अवस्था में लीन करने वाली उस शक्ति पर मनुष्यतारोपण करने पर वह 'शिव' कहलाती है। वह जो समस्त दृश्य-प्रपंच को छिन्न-भिन्न कर पुनः उसकी मूल अवस्था में लीन कर देता है, लयकर्ता है; परन्तु कहलाता संहारकर्ता है।
कोई वस्तु है और उसे समाप्त कर दिया जाये, तो मानवीय भाषा में कहा जाता है कि उसे नष्ट कर दिया। इस अर्थ में हम भी नित विनाशकर्ता ही हैं। इतना ही नहीं, यदि हमें एक गिलास फल के रस की आवश्यकता है, तो हम फल काट कर रस निचोड़ने वाले यन्त्र में डाल देते हैं और इस तरह हम फल को नष्ट कर देते हैं। यदि आप रस को शक्ति में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो रस को भी नष्ट करना होगा। और जो इसे शक्ति में बदलने हेतु गुटकता है, वह दानव बन जाता है। इस तरीके से प्रत्येक सृजन के लिए संहार-विनाश की अपेक्षा है।
-------------
१ इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् २ तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेत्ति तत्तेजोऽसृजत
शिव वह रौद्र शक्ति है जो उन सभी वस्तुओं को, जो रूपाकार हुई हैं, पुनः विसर्जित कर निराकार में लय कर देती है। ब्रह्मा सृजन करते हैं और बस, उनका इतना ही कार्य है। तब जब कल्पान्त होता है, शिव पधारते हैं और प्रलय कर देते हैं। ये दोनों कार्य दो छोर हैं और इन दोनों छोरों के मध्य सैकड़ों-हजारों वर्षों तक इन सृजित पदार्थों की, जीवों की देखभाल की जाती है, उनका पालन-पोषण तथा सुरक्षा की जाती है और उन्हें बनाये रखने के लिए आवश्यकीय सब-कुछ किया जाता है।
उसी शक्ति का दूसरा पक्ष (स्वरूप) इस योग क्षेम की चिन्ता करता है। युगों-युगों तक भूत, वर्तमान और भविष्य में उनकी देखभाल करने, वर्षा, धूप आदि आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने और समस्त विश्व-प्रक्रिया की छोटी-से-छोटी बात पर ध्यान देने तथा पालन, पोषण और रक्षण करने वाली इसी दिव्य शक्ति का अन्य रूप विष्णु है। दैवी शक्ति का यह रूप अनवरत क्रियाशील है। कोई समय ऐसा नहीं है कि वह हमारे जीवन से सम्बन्धित न हो और किसी समय वह हमसे उदासीन रहता हो। दिव्यता के सभी रूपों में से विष्णु अर्थात् नारायण की ही सर्वोपरि स्तुति की जाती है। इसका कारण है कि हम उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते।
इस विश्व में विष्णु की प्रिया लक्ष्मी खेतों में उगे अन्न के रूप में प्रस्तुत की गयी है; क्योंकि अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वह धन में भी मानी गयी है-धन जिससे संसार के समस्त क्रियाकलाप चलते हैं। वह समस्त सांसारिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, व्यापारिक ज्ञान आदि में निहित शक्ति मानी जाती है। अपने अष्ट-रूपों में वह नियमों का पालन कराने वाली विश्व में न्याय-व्यवस्था रखने वाली राज-शक्ति है। वह सबकी देखभाल करती है। उसका चिह्न हाथी है। हाथी राज-शक्ति का चिह्न है।
श्री भागवत पुराण में सृष्टि के रक्षक भगवान् विष्णु की महिमा का वर्णन है। उसके बारह स्कन्धों में से दसवाँ स्कन्ध अधिक बड़ा है। उसमें भगवान् विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का वर्णन है। उनका जन्म यमुना-तट पर बसी मथुरा नगरी में हुआ था। जन्म के तत्काल बाद उन्हें वृन्दावन ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अपनी किशोरावस्था अद्भुत लीलाओं में व्यतीत की।
उन्होंने अनेक साधु जनों की रक्षा की, दुष्टों का संहार किया तथा उन्होंने ही सर्वप्रथम विशाल जन-समूह में असली आध्यात्मिक प्रेम की तरंगें लहरा दीं। उन्होंने ही दिव्य सत्ता के प्रति भावात्मक प्रेम के बीज बोये और भक्तियोग का मार्ग बताया। भारत में भक्ति के सर्वश्रेष्ठ पात्र वे ही हैं। भक्तियोग उनके अवतार से प्रारम्भ हुआ है, जिसका मूल श्री भागवत है। सब भक्त भागवत के दशम स्कन्ध में वर्णित श्री कृष्ण की जीवनी से प्रेरणा ग्रहण करते हैं।
श्री कृष्ण की लीलाएँ हमारी प्रभु-भक्ति-भावना प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त, पूर्ण अवकाश देती हैं। हमारी उत्कृष्ट भावनाओं, भागवत भक्ति के भावावेगों तथा ईश्वर के प्रति हमारे शुद्ध प्रेम-भाव को अभिव्यंजित करने के लिए कृष्ण-लीला अधिकतम विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत करती है।
कृष्ण का जीवन, विशेषकर उनकी वृन्दावन-लीला, गोपी-प्रेम, भोले-भाले गोप-बालकों का प्रेम और साथ ही ईश्वर के प्रति मानव का गोप-बालकों जैसा निरीह प्रेम श्री कृष्ण के असंख्य भक्तों के लिए सदैव प्रेरणादायक रहा है।
भक्तियोग के मार्ग में आप भगवान् से कोई भावात्मक सम्बन्ध जोड़ कर भगवत्-साक्षात्कार करने की चेष्टा करते हैं। यह भावात्मक सम्बन्ध विविध साधनाओं द्वारा उच्चतम स्तर तक पहुँच जाता है और आपकी समस्त चेतना उससे इतनी परिप्लावित हो जाती है कि आप 'स्व' का ज्ञान भूल जाते हैं। आप स्वयं को ही भूल जाते हैं और स्वयं को भूल कर प्रेम-रूप हो जाते हैं। आप दिव्य प्रेम में बदल जाते हैं और इस प्रकार इन्द्रियों को पूर्णरूपेण भूल कर इस दिव्य प्रेम के द्वारा, जो आपकी चेतना को भी अनुप्राणित कर देता है, आरोहण कर ब्रह्मानुभव में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान् से, दिव्य सत्ता से यह प्रेम-सम्बन्ध कैसा हो सकता है, उसके कुछ रूपों का निर्देश किया जाता है। "जिसको मैं जानता नहीं, जिससे मैं अपरिचित हूँ, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, उसे मैं प्रेम कैसे कर सकता हूँ? वह दूर है, अपरिचित है, उसे कोई कैसे प्रेम करे?”
इसका प्रत्युत्तर भी प्रश्न-रूप में आया-"यहाँ तुम कैसे प्रेम करते हो? अपनी पत्नी को प्यार करते हो। पुत्र को, पुत्री को, बहन आदि को प्यार करते हो। अतः कठिनाई क्या है?"
उत्तर दिया जाता है-"यहाँ मैं इन सबको प्यार कर सकता हूँ; क्योंकि मैं उनको देखता हूँ, जानता हूँ और उनसे कोई सम्बन्ध ले कर जन्मा हूँ। अतः उन्हें प्रेम करना मेरे लिए स्वाभाविक है। उनसे दूर नहीं हूँ, उनसे अनजान या अपरिचित भी नहीं हूँ।"
यह समस्या है तो अवश्य ही; परन्तु हम आपके कथन को ही उद्धृत करके इसका समाधान करते हैं। आप कहते हैं कि 'वह अपरिचित है; अतः उसे कैसे प्रेम किया जाये?' परन्तु आप मनुष्यों को प्रेम कर सकते हैं; क्योंकि उनसे आप परिचित हैं। आप ऐसा कैसे सोचते हैं कि आप उससे अपरिचित या अनजान हैं? आप जिस प्रकार परिचितों और जाने हुए व्यक्तियों से सम्बन्ध जोड़ते हैं, उसी प्रकार से उससे भी जोड़िए। अतः किसी अजीब या नये तरह के प्रेम के सृजन की आवश्यकता नहीं है। आपको नये प्रकार का प्रेम जिससे परिचित न हों, खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसको विकसित करने के साधन ढूँढ़ने जाना है। किसी प्रकार के अस्वाभाविक या नवीन तरह के प्रेम की आवश्यकता नहीं। आपके हृदय में जिस प्रेम-भावना का प्राधान्य है, उसे ही भगवान् की ओर मोड़ दो।
एक कदम और बढ़ो। जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम था, भगवान् को उसी रूप में समझ कर उसी रूप में प्रेम करो जैसे उस व्यक्ति को करते हो। अतः यदि आप अपने बालक के प्रेमी हैं तो बच्चे के प्रति आपका जो प्रेम है, उसे ही ईश्वरोन्मुख कर दीजिए। यह न सोचिए कि वह तो भगवान् है, सर्वशक्तिमान् है, महिमामय है; बल्कि उसे अपना बालक मानिए, सरल भोला-भाला बालक मात्र। उसकी महिमा को, महानता को, विशालता को भूल कर केवल यही भावना कीजिए कि यह मेरा भगवत्स्वरूप बच्चा है।
मुझे विश्वास है कि बालक ईसा के सामने किसी को भी भय नहीं लगता होगा। इसके बदले जनता तो उस समय उसके प्राणों की रक्षा के लिए भी चिन्तित और भयभीत हो उठी थी जिस समय हेरोड ने बालकों की हत्या करना आरम्भ किया। वे लोग भी शिशु ईसा को छिपा कर मिस्र को पलायन कर गये। उन्हें लगा कि ईसा असहाय है और उन्हें सुरक्षा चाहिए। अतः उनकी जीवन-रक्षा के लिए वे उन्हें दूर ले गये। इस प्रकार उस छोटे से बच्चे के लिए उनके हृदय में वत्सलता का भाव था, वात्सल्य था। उस समय उनकी महिमा और महानता से जनता का कोई लगाव नहीं था।
इसी प्रकार जो भी सामान्य, स्वाभाविक मानवीय प्रेम-सम्बन्ध आपमें प्रबल हो, जिसमें आपकी हार्दिकता हो, वही सम्बन्ध भगवान् को दे डालिए। यदि आप उसमें से हैं जो अपने स्वामी को बहुत प्रेम करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को अपना ईश्वर मान लें। यदि आप अपने माता-पिता को प्रेम करने वाले बालक-बालिका हों, तो उन्हें माता-पिता समझ कर प्रेम करें। जितना प्रेम आपको अपने माता-पिता से है, उस समस्त प्रेम से उन्हें प्यार करें। इसी प्रकार अन्य किसी को भी यदि आप किसी दूसरे भाव से प्रेम करते हैं, तो उसी भावना से दिव्य सत्ता को प्रेम करें। इससे वह आपके और निकट हो जायेगा। तब वह आपके लिए अपरिचित, अनजाना या बहुत दूर नहीं रह जायेगा। प्रेम के क्षेत्र में इस प्रकार अपना विकास कीजिए।
भगवद्-भक्ति और प्रेम के पाँच तरीके सुझाये गये हैं जिनमें सबसे अधिक भावपूर्ण, गहरा आवेग-जनित प्रेम प्रियतम या प्रेयसी के प्रति होता है। प्रेम की यह भावना अत्यन्त तीव्र होती है। यदि आप सर्वाधिक इसी प्रेम से परिचित हैं तो कोई बात नहीं, आप भगवान् को अपना प्रियतम, अपने गहनतम प्रेम का पात्र ही समझ कर प्रेम करें।
श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम में प्रेम का यही रूप पूर्णता के उच्चतम शिखर तक पहुँचा हुआ है; परन्तु ध्यान रहे कि यह प्रेम मानव-आत्मा का दिव्य सत्ता के प्रति प्रेम का प्रतीक है। गोपियाँ भली-भाँति जानती थीं कि कृष्ण पूर्ण दिव्य सत्ता के, अक्षर ब्रह्म के प्रत्यक्ष साकार रूप हैं। इसी ज्ञान के कारण उन्होंने श्री कृष्ण पर अपना प्रेम न्यौछावर किया था। आप इसे कैसे जानेंगे? श्रीमद्भागवत का अध्ययन कीजिए। वह बतायेगा कि गोपियों के प्रेम की कैसे परीक्षा ली गयी और उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम कितनी अनुनय-विनय, पूजा-उपासना आदि करने पर प्राप्त हुआ। उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम सरलता से नहीं मिला, बड़ी तपश्चर्या के बाद मिला। वे शीतकाल में भी ब्राह्ममुहूर्त में चार बजे उठतीं और यमुना के हिमशीतल जल में स्नान करती थीं।
किसी ने उन्हें बताया था कि श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए अनेक सप्ताह तपश्चर्या और देवी की उपासना करनी होगी। अतः वे यमुना में स्नान कर ठिठुरती हुई मन्दिर जातीं और घण्टों देवी की पूजा करतीं। वे यह सब करती रहीं और साथ ही धी कृष्ण से अहर्निश निरन्तर प्रार्थना करती रहीं-"हमें वरदान दो कि हम सच्चे हृदय से आपको प्रेम कर सकें; आपके प्रति हममें सच्चा प्रेम भर दो और उसके प्रतिदान-स्वरूप अपना प्रेम दो।" और तब श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया- "अच्छा, मैं तुम लोगों से किसी पूर्णिमा की रात में मिलूँगा, तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान दूँगा तथा तुम्हें दिव्य प्रेम की महिमा दिखाऊँगा।"
उन्होंने मुरली बजायी और वे सभी गोपिकाएँ जब आयीं, तो मुरली की तान से बिलकुल मतवाली-सी हो रही थीं। मुरली की ध्वनि तो थी ही दिव्य और स्वर्गिक ! सैकड़ों गोपियाँ आ कर घिर गयीं। अचानक भोले से बन कर श्री कृष्ण कहने लगे- “तुम सबको क्या हो गया है? यहाँ क्यों आयी हो? तुम लोगों का यहाँ आना क्या उचित है? तुम विवाहित हो, घर में तुम्हारे पति हैं। क्या यहाँ आने के लिए तुम लोगों ने अपने पतियों से, माताओं या पिताओं से अनुमति ली है? रात्रि के इस प्रहर में अपने पतियों को तथा बच्चों को छोड़ कर इस प्रकार चली आना तुम जैसी युवतियों के लिए अच्छा नहीं है। यह बहुत अनुचित है। जनता क्या कहेगी? संसार क्या कहेगा? अतः लौट जाओ। कृपा करके घर लौट जाओ।" इस तरह वे आचार्य बन गये।
आप जानते हैं कि गोप-बालाओं ने उन्हें क्या उत्तर दिया? आप भागवत के दशम स्कन्ध में पढ़ें। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा- "तुम सोचते हो कि हम नहीं जानतीं कि तुम कौन हो? हम अपने पतियों को छोड़ कर कैसे आ सकती थीं ? पतियों में हम किसे प्रेम करती हैं? जिसे प्रेम करती हैं, वह क्या अन्तर्वासी नहीं है? हमारा प्रेम उसी अन्तर्वासी के लिए है और क्या तुम वही सबके अन्तर्वासी, सर्वान्तर्यामी नहीं हो? क्या तुम हिरण्यगर्भ परमात्मा, केवल सत्ता नहीं हो जो समस्त प्रेम और भक्ति को सारवान् बनाते हैं? हम जानती हैं कि तुम वही हो और यह जान कर ही तुम्हारे समीप आयी हैं। तुम्हारे प्रेम में मुक्ति है, गति है, मोक्ष है। तुम परम हो, अनन्त हो।" इस प्रकार वे कृष्या पर प्रकट कर देती हैं कि वे जिसके पास आयी हैं, उसे भली-भाँति जानती हैं।
जब वे कृष्ण के समीप पहुँचती हैं, उन्हें देह की सुध नहीं है। प्रेम में देह-बोध, देह-चेतना नहीं रह जाती। यह प्रेम सांसारिक नहीं होता, अतः उसमें भौतिकता नहीं होती। गोपियाँ जीवात्मा के रूप में पूर्ण रूप से जानती थीं कि कृष्ण विशुद्ध विश्व-प्राण पूर्ण ब्रह्म हैं; अतः उनके निकट देह-चेतना से मुक्त हो कर पहुँचती हैं और अपना प्रेम अर्पित करती हैं। यह इन्द्रियातीत नाटक है-दिव्य सत्ता के आवाहन पर मानव के अनुगमन का दिव्य नाटक। और फिर गोपियाँ तो स्वयं दिव्य अवतार थीं।
अतः वृन्दावन की गोपियों के समान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची निःस्वार्थ भक्ति-भावना का विकास करें। उसी में आपका परम श्रेय और सुख निहित है। भगवान् के प्रति अटल और अबाध भक्ति त्याग और विवेक दोनों लाती है। भक्ति ज्ञान-नेत्र खोल देती है। भक्ति और दीनता से भगवान् सहज द्रवित हो जाते हैं।
वृन्दावन-विहारी भगवान् कृष्ण आपको सुख और स्वास्थ्य प्रदान करें! ॐ नमो भगवते वासुदेवाय !
१९.पूर्णता का प्रवेश-द्वार
अध्यात्म के देदीप्यमान सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के प्रति मेरी श्रद्धांजलि! उनकी ज्योति सदैव प्रकाशित रहे! उस ज्योति का प्रकाश सम्पूर्ण विश्व के मानव-जीवन को प्रकाशित करता रहे!
दिव्य सत्ता की सौभाग्यशाली सन्तानो! आप यहाँ अपनी दिव्य नियति को प्राप्त करने आये हैं। यह दिव्य नियति पूर्णत्व से किसी भी प्रकार कम नहीं है। आपके समक्ष उज्ज्वल भविष्य है जो जीवन में परम तत्त्व तथा प्रभापूर्ण आध्यात्मिक सौन्दर्य की प्राप्ति के लिए गतिशील है। यह पूर्णत्व और यह सौन्दर्य-उपलब्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आपका मानव-जीवन इन दोनों तत्त्वों को विशुद्ध आध्यात्मिक सत्ता, ईश्वर के नित्य, पूर्ण और असीम दिव्य जीवन से निश्चित रूपमें ग्रहण करता है। आप आध्यात्मिक वैभव के उत्तराधिकारी हैं, दिव्य पूर्णत्व के उत्तराधिकारी हैं, अनन्त सौन्दर्य, असीम आनन्द और अनिर्वचनीय शान्ति के उत्तराधिकारी हैं।
यह वैभव, यह पूर्णता, यह सौन्दर्य, आनन्द और शान्ति आपका वास्तविक स्वरूप है। यह वास्तविक अन्तरात्मा है। यह दिव्यता आपकी वास्तविक सत्ता के भीतर है। आप दिव्य हैं, यह विश्व परम दिव्य सत्ता का अभिव्यक्त, प्रकटित रूप है। इस विश्व में आपका जीवन दिव्य प्रक्रिया ही है। अतः जीवन दिव्यता से यापन करें।
जीवन क्या है? अपने अन्तर के आध्यात्मिक तत्त्व का विकास और प्रकाश तथा नाम-रूपों के दृश्य में छिपी हुई दिव्यता का अनुभव और दर्शन करने का यत्न तथा प्राप्ति जीवन है। बाह्य जगत् को ईश्वर-रूप में देखना और इस प्रकट दिव्यता की अविराम निःस्वार्थ प्रेममयी सेवा द्वारा पूजा करना जीवन है। यह जो कुछ है, सब पवित्र है। दैवी सत्ता की उपस्थिति सब स्थलों और वस्तुओं को पावन बना देती है। आप जहाँ-कहीं भी हैं, वहीं उस परम भव्य के समक्ष हैं। जो-कुछ भी आप करते हैं, विश्व-नियन्ता के लिए, अव्यक्त परमेश्वर के लिए जो अपनी सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, उसके लिए करते हैं। अतः अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाइए।
जीवन को आध्यात्मिक बना लीजिए। पूर्णता में प्रवेश करने का यही द्वार है। यही महिमा का पथ है। यही परम उपलब्धि का रहस्य है। छोटे-से-छोटे विचार और भावना को, एक-एक शब्द और कार्य को, हरेक चीज को गहरे श्रद्धा, भक्ति और पूजा-भाव से भर दो। अपने समस्त जीवन में आध्यात्मिक भाव को परिव्याप्त होने दो और इस प्रकार अपने जीवन और कार्य को नवीन दिशा में बढ़ाओ । संसार में रहते हुए, भी आध्यात्मिक स्तर से जुड़े रहो। नवीन दृष्टि और नवीन गति धारण करो। अन्तर्यामी की चेतना में ही जीओ। ईश्वर की ज्योति का प्रकाश सर्वत्र देखो। भगवान् आपको समस्त नेत्रों से देखते हैं। संसार में रहना ईश्वर के सामीप्य में रहना है। यहाँ रह कर स्वयं को भगवान् में निविष्ट करो। ईश्वर इस क्षण भी यहीं है। सारा जीवन आध्यात्मिक है। अतः इस सत्य की अनुभूति करो। इस अनुभूति को दृढ़ करो। सत्य में जीवन बिताने का प्रयत्न करो। जागरूक हो कर अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने की चेष्टा करो। यही सौभाग्य की कुंजी है।
हमारे श्रद्धास्पद पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने स्वयं इस प्रकार का जीवन व्यतीत किया है और हमको भी यह पथ दिखाया है। उनकी दृष्टि में सब वस्तुएँ पवित्र थीं, पुनीत थीं, प्रत्येक क्रिया आध्यात्मिक क्रिया थी। उनकी दृष्टि में हरेक वस्तु अगणित रूपों में प्रकट हो रहे ईश्वर का स्वरूप थी। उनके जीवन में कर्म करना श्रद्धा करना था, कार्य पूजा था और जीना प्रार्थना थी। उनके लिए खान-पान, बोलना-सुनना, बैठना-चलना, आना-जाना आदि शरीर की साधारण सामान्य क्रियाएँ भी पवित्र क्रियाएँ थीं और इसलिए वे सब भगवान् के चरणों में अर्पित की जाती थीं। शरीर की प्रत्येक गति भगवान् की प्रार्थना या उसके अनवरत स्मरण के संग-संग होती थी। समस्त क्रियाओं के साथ-साथ दिव्य नाम का मौन जप चलता था। 'मैं तेरा हूँ, सब-कुछ तेरा है' यह उदात्त आन्तरिक भावना उनके हर एक कार्य में रहती थी। आध्यात्मिकता उनके जीवन का मूल मन्त्र था। अपने अनुयायियों के लिए उनका आदेश था- "जीवन को आध्यात्मिक बनाओ।" उनके उपदेशों का यही मर्म था। यही मानवता के प्रति उनके सन्देश का सार था। जो इसको अपनाता है, निश्चय ही मुक्ति की प्राप्ति करता है, पूर्णत्व को उपलब्ध होता है।
प्रिय साधको! ईश्वर प्रेम है और समस्त जीवन पवित्र है। जीना सनातन भगवान् की पूजा है। इसी कारण से आध्यात्मिक जीवन यापन करना आरम्भ कर दो। जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से भर दो। पूर्णत्व में प्रवेश का यही द्वार है। आप ईश्वर के समक्ष आ जाओगे, उनका साक्षात्कार कर लोगे।
सूर्योदय से पूर्व ही निद्रा त्यागें और इस विश्व-रूप ईश्वर को प्रणाम करें। दैनिक चर्या आरम्भ करने से पूर्व उसे प्रणाम करें, श्रद्धा में झुक जायें। पूजा-भाव से दिवस को भर दें। भक्ति-भाव से कार्य करें। समस्त नाम और रूपों में ईश्वर का दर्शन करें। शिष्ट और विनम्र रहें। कृपालु तथा उदार रहें। दयालु और सहानुभूतिशील रहें। क्षमा करके विस्मरण कर दें। सबके साथ भलाई करें। दूसरों की सेवा के लिए जीयें। अहं और स्वार्थपरता को उखाड़ फेंकें । जनसेवक बन जायें, सबकी आशा बन जायें तथा शान्ति और एकता के दूत बन जायें। सबके हित (कल्याण) और सुख के लिए जीयें और कर्म करें। क्रोध पर नियन्त्रण रखें। द्वेष को प्रेम से जीतें। सच्चे और ईमानदार रहें। कभी भी किसी को धोखा न दें, हानि न पहुँचायें, कष्ट न दें।
सदाचारी और परोपकारी बनने की ठान लीजिए। दूसरों की भलाई के कार्य में लग जायें; क्योंकि ईश्वर समस्त प्राणियों में निवास करता है। इन्द्रिय-विनिग्रह, मनोजय तथा लोभ और स्वार्थपरता के त्याग द्वारा अपनी उस दिव्य नियति की ओर, पूर्णत्व और मोक्ष की ओर बढ़ चलिए। उसे इसी जीवन में प्राप्त करिए और जीवन्मुक्त हो जाइए। जीवन क्षणिक है। समय भागा जा रहा है। अतः रुकें नहीं। विलम्ब न करिए। समय नष्ट न करें। तुरन्त खड़े हो कार्य में लग जाइए। अरे महिमामय दिव्यता! अपने जन्मसिद्ध अधिकार की माँग कर। आदर्श जीवन का विकास कर। सद्गुणों से आलोकित हो जा। दिव्यता से ज्योतिर्मय बन जा और पूर्णत्व की ओर पग बढ़ा।
ईश्वर आपको शान्ति, आनन्द और ज्ञान का प्रकाश दें! पूर्णता के पथ पर आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो! आध्यात्मिकता के मार्तण्ड, हमारे प्रकाश के प्रकाश महा-सद्गुरु शिवानन्द की जय हो!
२०.गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज
सद्गुरु वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। वे वास्तव में परम अव्यक्त ब्रह्म के व्यक्त स्वरूप हैं। उन अपने आध्यात्मिक गुरु, निर्देशक और दिव्य गुरु को श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम कर उन्हें अपनी आदर-भावना अर्पित करता हूँ।
गुरु-प्रवर श्री स्वामी शिवानन्द का जन्म १८८७ ई. में हुआ था। उन्होंने ऋषिकेश के अपने पुनीत निवास-स्थान से जीवन का रूपान्तरण करने वाली आध्यात्मिक ज्ञान की जीवन के परम आध्यात्मिक आदर्श के ज्ञान की, इस अमूल्य मानव-जीवन के परम उद्देश्य के ज्ञान की-अजस्र धारा प्रवाहित की। उन्होंने वस्तुतः ज्ञान-गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान-गंगा बहा दी; क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवाह जो अध्यात्म, धर्म, संस्कृति आदि पर अनवरत लेखों के रूप में ऋषिकेश के उनके निवास-स्थल से निःसृत हुआ, उनमें निहित ज्ञान के द्वारा विश्व के समस्त देशों में, वहाँ की जनता में अध्यात्म की, जागरण की, आध्यात्मिक आकांक्षा की लहर फैल गयी और यह महान् आत्मा, जिसका सम्पूर्ण विश्व अध्यात्म-क्षेत्र में महा-सन्त के रूप में मान कर आदर करता है, चालीस वर्षों तक अथक अविराम गति से विश्व की छोटी-से-छोटी क्रिया और दैनिक जीवनचर्या के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन का, दिव्य जीवन का, हमारे अन्तर की दिव्य तत्त्व की अभिव्यंजक दिव्य पद्धति के अनुसार यापन किये गये दिव्य जीवन का, देश-देशान्तर के महान् सन्तों, ऋषियों, रहस्यदर्शियों की उदात्त पद्धति के अनुसार यापन किये हुए जीवन का, नीति, श्रद्धा, भक्ति और पूजा के जीवन का सन्देश देते रहे।
यही सन्देश यह सेवक समभागी होने की भावना के साथ आपको परम आनन्दपूर्वक अर्पित करता है। यदि आपको इन लेखों में कोई सार्थक वस्तु मिलती है, आपके दैनिक जीवन में कोई काम में आने योग्य तत्त्व इस सेवक के लेखों से मिलता है, तो उसके लिए हम अपने गुरु महाराज के प्रति ही कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे; क्योंकि यह उन्हीं का सन्देश है। यह सेवक तो केवल सन्देशवाहक है। आइए, हम सब मिल कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता एवं भक्ति व्यक्त करें जिनके शुभ जन्म-दिवस की तिथि ८ सितम्बर है।
इस महान् आत्मा ने स्फटिक जैसे शुद्ध जल वाली ताम्रपर्णी सरिता के तट पर बसे दक्षिण भारत के एक ग्राम में एक कुलीन ब्राह्मण के यहाँ सन् १८८७ में जन्म लिया था। आदर्श शैशव और प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थी-जीवन के पश्चात् इस आदर्श युवक ने, जिसका हृदय दया, पवित्रता, सत्यता और एकता की भावना से भरा था, चिकित्सक का पेशा अपनाया जो उसे सुदूर मलेशिया के तट तक ले गया। वहाँ बारह वर्ष तक वे अथक परिश्रम से, दिन-रात कष्टों से, रोगों से पीड़ित वहाँ के अगणित लोगों की सेवा करते रहे। उनका हृदय विशाल हो गया, सभी के प्रति प्रेम से पूर्ण हो गया। उनमें सहानुभूति पैदा हुई। दु खित जनता के लिए उनका हृदय करुणा से भर गया। उनकी दृष्टि में विभिन्न जातियों और वर्गों के लोगों में कोई भेद नहीं था। भारतीय, मलय, चीनी, जापानी आदि सबको उन्होंने एक-समान सम-भाव से अपना प्रेम दिया और उनके कष्ट और संकट की घड़ियों में राहत दी।
मानव-जीवन की विपन्नावस्था, उसके कष्ट, दुःख और वेदना के निकट सम्पर्क में आने के कारण इस सद्विचार वाले युवा पुरुष के जीवन में दिव्य संकल्प का उदय हुआ। कष्ट-पीड़ित जनता का चिकित्सक होने के उपरान्त वह शीघ्र ही उच्चतर जीवन की ओर उन्मुख हो संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुआ। और इस प्रकार विश्व में एक ऐसे आध्यात्मिक चिकित्सक का प्रादुर्भाव हुआ जिसने मानवात्मा को कष्ट से मुक्त करने का बीड़ा उठाया और दुःखियों को दुःख से अतीत, कष्ट से अतीत वह पथ दिखाया जो अमर जीवन, स्थायी शान्ति और आनन्द, परम शाश्वत कल्याण की ओर ले जाने वाला था। अतः चिकित्सा-जगत् और भौतिक जगत् ने जिसे खोया, वह आध्यात्मिक जगत् को उपलब्ध हो गया। जिसे मलेशिया के एक छोटे से समुदाय ने खो दिया था, वह समस्त मानवता को उपलब्ध हो गया।
वह वस्तुतः महत्त्वपूर्ण दिवस था जिस दिन डा. कुप्पू स्वामी संन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो स्वामी शिवानन्द बन गये। उसी दिन से उनका जीवन पूर्णरूपेण ईश्वर को समर्पित हो गया। गंगा के तट पर अनेक वर्षों तक घोर तपस्या करने के उपरान्त तथा कठोर आत्म-संयम और त्याग का, एकान्तवास का जीवन व्यतीत करने के दस वर्ष के उपरान्त भगवान् के प्रकाश से परमानन्द से पूर्ण दिव्यात्मा हो वे बाहर आये।
मानवता के प्रति प्रेम और करुणा से उनका हृदय उसी प्रकार उद्वेलित हो रहा था जिस प्रकार ढाई हजार वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का हुआ था और वे अपने उस अद्भुत ज्ञान को, आनन्द और शान्ति को अपने सभी सजातीय लोगों में बाँटने की इच्छा ले कर चल पड़े। इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या और ध्यानोपासना से, मौन तथा पार्थक्य से, कठोर आत्म-संयम और एकान्तवास से सन् १९३० में बाहर पग रख कर जीवन के आध्यात्मिक आदर्श के सारभूत ज्ञान और सांसारिक जीवन के दैनिक ऊहापोह में भी इस आदर्श को उपलब्ध होने की विधि का ज्ञान प्रदान करने जैसा महान् आध्यात्मिक कार्य आरम्भ कर दिया।
जीवन में ही आध्यात्मिक आदर्श उपलब्ध कर लेना-यही उनका महान् सन्देश था। न तत्त्व-चिन्तन, न दर्शन, न वाद-विवाद व रूढ़ियाँ, न मत-मतान्तर, न रीति-रिवाज कुछ नहीं; बस केवल व्यावहारिक दिव्य जीवन यापन, उस भगवान् की दिव्य शक्ति की सर्वव्यापकता के ज्ञान से पूर्ण जीवन, जो समस्त जीवों का उद्भव (कारण) है, उससे स्वयं की नित एकता और नित सम्बन्ध का जीवन।
ऐसा जीवन यापन केवल अरण्यों में, गुहाओं में, पर्वत-शिखरों पर अथवा एकान्त निर्जन में ही हो, यह आवश्यक नहीं। यह तो हर जगह-घरों में, कार्यालयों में, बाजारों में, जन-समूहों में कहीं भी और कभी भी यापन किया जा सकता है। यह तो परिवर्तित व्यक्ति का अध्यात्म-केन्द्रित गतिशील जीवन यापन है दैनिक जीवन-व्यापारों के बीच से गुजरते हुए उस गौरवपूर्ण उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति की, परम लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा में संलग्न जीवन यापन है। ऐसा जीवन यापन दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने पर, सभी को दिव्य और शुद्ध मानने तथा समस्त कार्य को अनन्य पूजा और समर्पण समझ लेने पर सम्भव होता है। दिव्य जीवन का यही रहस्य है।
हमारी भावनाएँ उन्हीं को अर्पित हैं जिन्होंने अध्यात्म-सन्देश के अधिकाधिक प्रचार और प्रसार का इतना अधिक प्रयत्न किया, जिन्होंने अपने चतुर्दिक् प्रेरणा-प्राप्त, उत्साही, समर्पित युवा कार्यकर्ताओं का एक उपनिवेश-सा बना लिया, जिन्होंने दिव्य जीवन के सन्देश के प्रचार हेतु दिव्य जीवन संघ को रूपरेखा दी और जिन्होंने अखिल विश्व को अपना आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान प्रदान किया।
जिन क्षणों में हम ऐसे महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे क्षण बड़े ही भाग्यशाली हैं। वह प्रहर भी भाग्यशाली है जिस प्रहर हम ऐसी महान् विभूतियों का सम्मान करते हैं। हमें महापुरुषों की जीवनियों से प्रेरणा मिलती है। वे जैसे हमें स्मरण कराती हों कि हम भी अपना जीवन उनके जैसा ही उदात्त बना सकते हैं। स्मरण रखिए, ऐसे दिव्य पुरुषों का चिन्तन करने से उनकी जीवनी हमारे भीतर प्रेरणा भरती है और हमें उनके चरण-चिह्नों का अनुकरण करने हेतु, उनके आदर्शानुसार जीवन यापन हेतु, उस आदर्श की प्राप्ति हेतु जिसके वे साकार रूप थे तथा उनके उपदेशों को सुनने के लिए हमें विकल कर डालती है।
मैं अपार हर्ष के साथ आप सबके लिए आध्यात्मिक प्रयत्न और साधना का, नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति का तथा उदात्त पूर्णता का भव्य जीवन यापन करने की शुभ कामना करता हूँ। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के नाम पर, जिनके चरणों में हम सब श्रद्धापूर्वक इकट्ठे बैठते थे, मैं आपके लिए इसी जीवन में भगवद्-साक्षात्कार जैसी दिव्य उपलब्धि की कामना करता हूँ। गुरुदेव के समान महान् सन्त को हम सर्वाधिक श्रद्धा-भाव जो दे सकते हैं, वह यही कि उनके उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। जो सबसे बड़ी श्रद्धा या सम्मान हम महान् आत्मा को दे सकते हैं, वह यही है कि उनके सद् उपदेशों को हृदयंगम करें और उनके अनुसार चलें। उनके अपार अनुग्रह से उऋण होने का एकमात्र स्वरूप यही होगा कि हम बड़ी लगन से विनम्रतापूर्वक उनके चरण-चिह्नों पर चलें। आज हम उनके उपदेशों की भावना के अनुसार जीवन यापन के निश्चय के रूप में उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करें। आप सबको भगवत् आशीर्वाद प्राप्त हो!
गुरुदेव शिवानन्द जी की जय हो ! समस्त सन्तों और गुरुओं की जय हो! उनका आशीर्वाद आप सब पर हो! दिव्य जीवन यापन करके आत्म-साक्षात्कार कीजिए! आप सब पर गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव रहे!
२१.भक्ति-मार्ग
ऐसे साधकों का संग होना जो ईश्वर-भक्त हैं और दिव्य चेतना के आकांक्षी है, स्वयं में ही एक महान् उपलब्धि है। मुमुक्षुओं का संग प्राणों में पुनर्जीवन भरने, आध्यात्मिक भावना की शक्ति से सम्पन्न बनाने और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा हम परिवर्तनशील नाम-रूपों के पीछे जो अपरिवर्तनीय तत्व है, उसके आन्तरिक बोध को पुनः ताजा करते हैं और उसके साथ पुनः सम्बन्ध जोड़ते हैं जो हमारे प्राणों का प्राण है, हमारी सत्ता का मूल उद्गम है, हमारा परोक्ष आधार और हमारे अस्तित्व की अन्यतम गति है। इस सत्संग द्वारा आप एक बार पुनः अपनी आन्तरिक कड़ी को परम दिव्य के साथ प्रभावशाली ढंग से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। सत्संग का यही प्रयोजन और अभिप्राय है अर्थात् उसके निकट-से-निकट सान्निध्य में चले आना जो अन्तर्यामी है, नित है, अव्यय है, सर्वदा पूर्ण है और ऊहापोह से पूर्ण इस नाम-रूपों के अपूर्ण और क्षणिक संसार के प्रतिबिम्ब का अखण्ड आधार है। अपने सम्बन्ध को उससे पुनः जोड़िए जो सर्वव्यापी सत्य और आपकी सत्ता की अन्तरात्मा है।
सत्संग का विशिष्ट महत्त्व इसी में निहित है; क्योंकि यह आपकी चेतना को क्षणभंगुर असत्यता से उस मूलभूत सत्य में ले जाता है और समस्त दृश्य अनुभूत्यात्मक जगत् का आधार है। इस जीवन्त सम्पर्क में, इस अविच्छिन्न और अनवरत सम्बन्ध में, इस सुदृढ़ आत्मिक सम्बन्ध में ही जीवन की वास्तविक सम्पूर्ति का आश्वासन है। इस आध्यात्मिक सम्बन्ध को, इस आन्तरिक सम्बन्ध को तोड़ दीजिए और तब देखिए कि आपका जीवन नीरस, निस्सार तथा मरुभूमि सदृश्य हो रहेगा; अन्धकार से, खेद से, नैराश्य से, रिक्तता और सूनेपन से भर उठेगा। सत्य से जिसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसका जीवन अपना अर्थ खो बैठता है। यह सत्य का अर्थ छद्मवेशी सत्य से नहीं, बल्कि उस सत्य से है जो आपकी सत्ता का मूल है। वही आपके अस्तित्व का स्रोत है। अतः वह सम्पर्क जीवन्त तथ्य है जो जीवन को अर्थवान्, महत्त्वपूर्ण, गम्भीर, पूर्ण और प्रखर बनाता है।
वृक्ष का ही दृष्टान्त लीजिए। धरती से बहुत ऊँचाई पर उसमें फल, फूल तथा पत्ते होते हैं जो जीवन की ताजगी लिये हैं, शक्तिवान् हैं तथा विकास पा रहे हैं। अन्तरिक्ष में इस जीवन का क्या रहस्य है? दृष्टि से ओझल, दिखायी न पड़ने वाले और इसलिए समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों की दृष्टि से अस्तित्वहीन, परन्तु जीवन-ऊर्जा के किसी स्रोत को निहित किये हुए। धरती के भीतर गहराइयों में छिपा यह जीवन और पोषण का स्रोत ही उसे बढ़ने की शक्ति देता है। वृक्ष के ये विविध भाग, पृथ्वी से चाहे कितनी ही ऊँचाई पर क्यों न हों, उस अदृश्य स्रोत से उनका छिपा हुआ सम्बन्ध होता है और यही उनके जीवन का रहस्य है। यदि आप किसी शाखा को काट डालें, किसी टहनी को झुका कर तोड़ दें, वृक्ष से अलग कर दें, तो उसके पुष्प और पत्ते तुरन्त मृत हो जायेंगे और शीघ्र ही सूख जायेंगे।
इसी प्रकार आपके जीवन के सम्बन्ध में भी है। जो-कुछ विधेयात्मक (Positive) है, उस सबका एक अदृश्य स्रोत, एक गुप्त कोश है। जब दुःखातीत आनन्द से आपका जीवन क्षोभों और उद्वेगों से परे शान्ति में पुष्पित होने लगता है, उस चेतना की ज्योतिर्मय अवस्था में जो इस अर्ध सत्य, अज्ञान और त्रुटि से बहुत ऊँचे हैं, प्रवेश करने लगता है, तब आप उस स्रोत को उपलब्ध हो जाते हैं जो आपको जीवन के ध्येय की ओर अग्रसरण की गति देता है। उसे आत्मा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। आप चाहे जिस नाम से पुकारें, यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते और यदि उपेक्षा करते हैं तो अपने सुख, शान्ति, पूर्णता की भावना और संक्षेप में कहा जाये तो अपने प्राणों की बाजी लगा कर ही उपेक्षा कर सकते हैं।
एक बड़े सन्त ने जीवन के तथ्य के रहस्य को एक वाक्य में कहा था- "ईश्वर का स्मरण जीवन है और उसकी विस्मृति मृत्यु।" व्यक्ति ज्यों-ही उस दिव्य से अपना सम्बन्ध तोड़ कर अलग होता है, उसके जीवन की गति में अवरोध आना आरम्भ हो जाता है और जीवन उसके लिए भार हो जाता है। वह आनन्द का संगीत, सौन्दर्य की प्रतिमा और अभ्युदय एवं बाह्य विकास का साधन नहीं रह जाता। अपने स्रोत से, विश्वात्मा से कट कर इस सीमित क्षुद्र अहं-भाव के कारण जीवन दुःख, वेदना और यातनाओं का भार मात्र रह जाता है।
उस दिव्य से अपना सम्बन्ध बनाओ अथवा उससे अपने सम्बन्ध की याद रखो (यह सम्बन्ध ऐसा नहीं है जिसे बनाना पड़े, प्रत्युत उसका ध्यान रखना है, विस्मरण या उपेक्षा नहीं करनी है)। याद रखिए, अपने वास्तविक स्वरूप में आप सदैव ही अपनी सत्ता के दिव्य स्रोत से जुड़े हैं। क्रमिक रूप में अपना यह सम्बन्ध और घनिष्ठ तब तक बपाते जाइए, जब तक ईश्वर ही आपकी चेतना का प्रधान और प्रभावशाली तत्त्व नहीं बन जाता अर्थात् आपकी चेतना भागवत चेतना नहीं बन जाती । यही परमावश्यक है। यही पूजा है और जीवन को वस्तुतः पूर्ण और सच्चे अर्थों में उपलब्धियों के द्वारा सफल बनाने का, इस क्षणिक परिवर्तनशील पार्थिव जीवन के दोषों और अपूर्णताओं को अतिक्रमण करने का यही उपाय है।
समस्त धर्म, समस्त पूजा का ध्येय अपनी सत्ता के इस महा तथ्य को पुनर्नवीन करना और उसकी पुनर्प्राप्ति करना है- "मैं इस संसार की अपेक्षा लाखों गुणा अधिक भगवान् का अपना हूँ। संसार से मेरा सम्बन्ध मात्र क्षणिक है। कुछ ही देर पूर्व मैं इस विश्व का नहीं था, न मैं इस विश्व के लिए हूँ। अभी मैं यहाँ हूँ, परन्तु मुझे शीघ्र ही यहाँ से चले जाना है। एक क्षण ऐसा आयेगा कि इस बाह्य प्रपंचात्मक संसार से मेरा सम्बन्ध समाप्त हो जायेगा और मैं पुनः उसी आयाम में वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ से इस बाह्य प्रपंच के अस्थायी सम्पर्क की अवस्था में प्रवेश किया था।"
मानव भी कैसा अन्धा है! कभी सत्य को नहीं देखता। माया विविध प्रकट रूपों में प्रत्यक्ष हो कर सत्य के महत्त्व को धारण कर रही है और इस प्रकार मनुष्य को सत्य का विस्मरण करा रही है। उत्तरोत्तर गहरे; आन्तरिक आत्मिक सम्बन्ध की अवस्था में विकास और वर्धन पाने वाली तथा इस तथ्य का ज्ञान कराने वाली कि इस परिवर्तनशील, क्षणिक भौतिक क्रिया से हमारे सम्बन्ध की अपेक्षा भगवान् के साथ हमारा सम्बन्ध सहस्रों गुणा अधिक वास्तविक और सार्थक है, यह प्रक्रिया एक आवश्यकीय महान् प्रक्रिया है विशेषकर उस स्थिति में जब आप अपने जीवन में सचमुच ही आनन्द, पूर्णता, शान्ति, वैभव, सौन्दर्य, सन्तुलन और स्वास्थ्य चाहते हों।
समस्त धर्म, मत और सम्प्रदाय तथा सन्त केवल इसी महान् लक्ष्य को ले कर संसार में आये हैं-मानव को इस जीवन में अपने इस सम्बन्ध को अधिक गत्यात्मक एवं जीवन्त बना लेने की आवश्यकता का पुनः स्मरण दिलाने आये हैं। समस्त धर्मों का यही मुख्य उद्देश्य रहा है और समस्त सन्तों का, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के, प्राचीन हों या आधुनिक यही मूल सन्देश रहा है। दर्शन और धर्मशास्त्रों का प्रमुख ध्येय रहा है व्यक्ति को इस नित परिवर्तनशील से, अनेकों की इस कलाबाजी से दूर करके उस स्थायी और अपरिवर्तनशील की ओर उन्मुख करना।
संसार के इस बीहड़ वन में स्वयं को खो नहीं देना है प्रत्युत अन्तर के देवालय की ओर चलना है जहाँ सौभाग्य का निवास है। धर्म का मुख्यतः यही आशय है। धर्म के समस्त अनुष्ठान, सभी योगाभ्यास तथा आचार्यों, गुरुओं आदि द्वारा उपदिष्ट सभी प्रविधियाँ केवल एक ही उद्देश्य अथवा लक्ष्य ले कर चली है और वह है स्वयं को अ सत्ता में, अन्यतम सत्ता में, अद्वितीय सत्य में, जिसके विषय में ही वास्तविक रूप में कह सकते हैं, 'यह मेरा है और मैं इसका हूँ' पूर्णता के साथ पुनर्स्थापन।
विश्व की अन्य किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में आप इस सत्य को निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वह मेरा है और मैं उसका हूँ। अपने शरीर के सम्बन्ध में भी नहीं कह सकते, चाहे वह शरीर आपको कितना ही प्रिय क्यों न हो, चाहे वह आत्मा के समान ही निकट क्यों न हो और चाहे आपने उससे पूर्ण तादात्म्य ही क्यों न कर लिया हो। शरीर भी आपको एक दिन आपत्ति काल में छोड़ कर यह कहता हुआ चला ही जायेगा- "मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं यहाँ किसी अन्य विधान, कर्म-विधान के वश में हूँ और जब यह कर्म पूरा हो जायेगा, तुम अपना कह कर मुझ पर दावा नहीं कर सकोगे।"
जब आप शरीर को अपना समझते भी हैं, तब भी उस पर आपका कितना नियन्त्रण रहता है? भोजन में कोई भी गलत चीज खा लेने पर पेट में गड़बड़ी हो जाती है। उस समय क्या आप कह सकते हैं- "तुम मुझसे सम्बद्ध हो, अतः गड़बड़ मत होओ, गड़बड़ी बन्द कर दो!" वह आपकी बातों पर कान नहीं देगा। आप शोध करके चाहे डाक्टर (पी-एच.डी.) की तीन उपाधियाँ ले लें, चाहे देश के राष्ट्रपति ही क्यों न बन जायें, शरीर पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आप उसके प्राकृतिक कार्यों के अनुकूल चलते हैं और उससे ठीक ढंग से व्यवहार करते हैं, तब वह आपके साथ चलेगा। अन्यथा यदि आप उसके किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, तो वह आपको बता देगा कि आपका उस पर कितना नियन्त्रण है। अतएव, हमें जानना है कि केवल एक ही सत्ता सत्य है जिसको हम दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं- "तू मेरा है और मैं तेरा हूँ।" और सत्ता है भी वही।
ईश्वर आपका अपना है। दिव्य आपका अपना है। उससे आपका शाश्वत सम्बन्ध है। आपकी सत्ता उसी में है। अतः जीवन में परमावश्यक है उससे घनिष्ट सम्बन्ध रखो जो नष्ट नहीं होता, जिसका अन्त नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो आपको कभी निराश नहीं कर सकता, आपके जीवन में भ्रम पैदा नहीं कर सकता। अनित्य के साथ के सभी सम्बन्ध अन्ततः दुःखद होते हैं। वह निरीह सत्य है। यदि आप किंचित् चिन्तन करें, तो सामान्य बुद्धि से पता चल जायेगा कि अनित्य का संग अन्ततः दुःखपूर्ण होता है और वह शाश्वत सत्ता ही एकमात्र है जो आपकी अन्तरतम अभिलाषा पूर्ण कर सकती है। शाश्वत सत्ता ही आत्मा को सन्तोष दे सकती है और आप आत्मा हैं। आप यह भौतिक शरीर नहीं हैं। आप यह सदैव चंचल रहने वाला मन नहीं हैं, और न ही बुद्धि तथा न यह मिथ्या क्षुद्र अहं हैं।
आप आत्मा हैं; अतः केवल नित्य ही आपकी अभिव्यक्ति को सन्तोष देगा। आप नित्य में ही वास्तविक आनन्द, वास्तविक तृप्ति, वास्तविक शान्ति और बास्तविक अर्थ में सर्वथा पूर्ण होने की भावना प्राप्त कर सकेंगे। यही एक भावना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, सदैव इसी के निकट रहना चाहिए, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए और इसके साथ अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध रखना चाहिए और इस सम्बन्ध को सदैव गत्यात्मक और संवर्धनशील होना चाहिए।
आप इसे किस प्रकार कर सकेंगे ? आपको जो क्षमताएँ प्राप्त हैं, उनके द्वारा ही कर सकते हैं। आपके औजार वे ही हैं। यदि अन्य वस्तुओं की भाँति दैवी सत्ता भी स्थूल स्पर्शनीय होती, तो सर्वप्रथम आप उसे अपने शरीर द्वारा पकड़ते और पकड़े रखते; परन्तु वह तो अति-भौतिक और अदृश्य है। कम-से-कम आपकी वर्तमान चेतन-अवस्था के लिए तो वह अभौतिक और अदृश्य ही है। सम्प्रति आपकी चेतना बहिर्मुखी प्रतिस्थापित विचार, वस्तुपरक अनुभूति है। अतः आपको संसार ही दिखायी देता है।
वह कौन है जिसने आपको विश्व-प्रक्रिया के संग, बाह्य विषयपरक जगत् के साथ उलझाव की स्थिति में पहुँचाया? और कैसे आप विविध वस्तुओं और अनुभवों में फँस गये हैं जिनसे आप स्वयं को मुक्त नहीं कर पायेंगे? आप अपनी भावनाओं और भावुकता के कारण ही बँधे हैं और आसक्त हुए हैं। उन्होंने आपको आपके ही राग और आसक्ति के काँटे में फँसाया है।
व्यक्ति का स्वभाव जो प्रच्छन्न भावुकता और व्यक्तित्व से बना है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस वर्तमान लिप्तता का जो बन्धन है, दासता है और विषय अनुभव में स्वयं को खो देना है, इसका (लिप्तता का) मुख्य कारण और प्रवृत्त करने वाली शक्ति वही है। अतः इस लिप्तता (Involvement) से उदित होने वाली समस्त स्थितियों के अनुभवों के समक्ष स्वयं को उद्घाटित करके एक प्रकार से मनुष्य स्वयं को इस लिप्तता से उत्पन्न नाना प्रकार के अनुभवों के समक्ष उद्घाटित कर देता है। सुख में, दुःख में, कष्ट में, यातना में, सफलता तथा भग्नाशा में समान रूप से प्रकट कर देता है। अतः बाहरी जगत् के प्रति आपकी लिप्तता आपकी भावुकता द्वारा अनिवार्य रूप से प्रकट होने के कारण आपमें सदैव प्रतिक्रिया होगी और वह आपकी सत्ता के उस आयाम तक होगी जहाँ आपके व्यक्तित्व का संवेदनशील तत्त्व है।
२२. अध्यात्म-विद्या का सार
परम पिता परमात्मा को, अगणित सृष्टियों के सर्वशक्तिमान् नियन्ता को, प्रेम के परमेश्वर को कोटिशः प्रणाम। जिसकी कृपा से आज इस प्रातः हम सब एकत्र हुए हैं, उस प्यारे पिता को मेरा प्रणाम और साष्टांग दण्डवत्। इस प्रात: वेला में, इन क्षणों में हम सब आपका अनुभव करें। देवाधिदेव! हम विनम्र सेवा-भाव से, यहाँ आपके प्रति सामान्य प्रेम-भाव से एक-दूसरे के निकट सान्निध्य में आये हैं, आने का प्रयत्न किया है। आध्यात्मिक भावना से मिलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं तथा स्वीकार करते हैं कि इस आध्यात्मिक सम्पदा को प्रदान करने की जो कृपा आपने की है, वह इसलिए नहीं कि हम अपने गुणों के कारण उसके योग्य हैं, प्रत्युत हम अकिंचनों के प्रति आपने अपने अपार प्रेम, यदृच्छ कृपा तथा असीम अचिन्त्य करुणा के कारण ही दर्शायी है। हमारे प्रति जो आपने यह महान् कृपा और दया की है, उसके हम बिलकुल भी योग्य नहीं हैं। आपका नाम सदैव गौरवान्वित रहे !
मैं मदुरै की दिव्य जीवन संघ की शाखा को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे आप जैसे ईश्वरोन्मुख जीवन-पथ के पथिकों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्रदान किया। अध्यात्म-ज्ञान के इस पावन क्षेत्र में आ कर मुझे सन्तोष मिला है। इसी के साथ मैं प्रिय और आदरणीय बन्धु सेल्वामणि को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मदुरै आने पर मुझे यहाँ प्रेमपूर्वक आमन्त्रित करने की कृपा की और इस प्रकार मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे ईश्वर के विषय में कुछ कह सकूँ, अपने विषय में कह सकूँ तथा उससे (ईश्वर से) अपने सम्बन्ध के विषय में भी कह सकूँ जो हम सबका स्रोत है, आधार है और अन्तिम लक्ष्य है। अन्त में मैं आप सबको, जो आज ईश्वर की प्रेरणा से यहाँ एकत्र हुए हैं, धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ ईश्वर के एक विनम्र सेवक और स्वामी शिवानन्द जी के विनीत शिष्य के रूप में उपस्थित हुआ हूँ।
श्री स्वामी शिवानन्द जी विरले ही व्यक्ति थे जो एक धर्म-विशेष में जन्म ले कर उसी की आस्था और विश्वासों में पले; परन्तु उसके उपरान्त एक ऐसे आध्यात्मिक स्तर पर पहुँच गये जिसने उन्हें स्वतः ही उस धर्म से उठा कर एक ऐसी भूमिका पर ला खड़ा कर दिया जहाँ उन्होंने अनुभव किया कि वे किसी एक धर्म के अनुयायी नहीं रहे, प्रत्युत उस विश्व-धर्म के हो गये जो समस्त धर्मों के हृदय में छिपा है; अतः ईसाइयत या इस्लाम में उन्हें ऐसा ही लगता था जैसा हिन्दू-धर्म में। सब धर्म या मत उनके लिए एक जैसे ही थे। वे कहा करते थे कि धर्म केवल एक ही है और वह है जो जीव को पुनः ईश्वर की ओर ले जाना चाहता है। अतः वह ससीम की असीम की ओर, व्यक्ति की समष्टि की ओर, मानव की दिव्यता की ओर तथा मनुष्य की ईश्वरत्व की ओर यात्रा है। सभी धर्मों के अन्तर में इसी की खोज है।
मानव मात्र में आत्मा की गति भी उस सत्य के अनुभव में उठ कर उसे पकड़ने और उसमें अनुप्रविष्ट होने के लिए है जो (सत्य) अनादि है, अनन्त है, शाश्वत है, नित्य है, जो सदैव था, है और जिसका कभी अन्त नहीं होगा तथा जो इस स्थूल भौतिक जगत् का निर्माण करने वाली, परिवर्तनशील एवं क्षणिक दिखायी देने वाली वस्तुओं और नाम-रूपों में निहित है। इन अदृश्य होते हुए नाम और रूपों के पीछे कोई तत्त्व है। ये परिवर्तनशील परिवर्तनहीन के संग हैं। ये (नाम-रूप) अनित्य हैं, परन्तु वह नित्य शाश्वत सत्य है। उसे हम ईश्वर कहते हैं। उन्होंने कहा- "वही हमारा अन्तिम लक्ष्य है, वही अन्तिम गन्तव्य है। समस्त धर्म मनुष्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के योग्य बनाने का प्रयत्न करते हैं, उस तक पहुँचने में सहायता करते हैं।"
यह निश्चित है कि उन्हें धर्म का तत्त्व मिल गया था। उनका कहना कि धर्म के मूल-तत्त्व से भिन्न प्रचलित धर्म का बाह्य कलेवर बनाने वाले जो अन्य तथ्य हैं, वे उस धर्म-पद्धति का प्राण-तत्त्व नहीं होते, बाह्य कलेवर मात्र होते हैं। मानवात्मा की उस सनातन सूक्ष्मातिसूक्ष्म परम सत्ता और सनातन, अचिन्त्य, सूक्ष्म अलौकिक तत्त्व की और सुनिश्चित गति ही धर्मपरायण जीवन है और उस तत्त्व का कोई नाम नहीं है।
वह अनाम है। उसे हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। उसके असंख्य नाम हैं। साथ ही वह नाम-रहित भी है। वह जो है, वही है (It is that which is)। इसी को उद्घोषित करता हुआ वह कहता है- "मैं जो हूँ, वही हूँ (I am that I am) ।" यह जानते हुए कि मैं वही हूँ जो नित्य है, शाश्वत है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य कालातीत नित्यता में बदल जाते हैं । वह मैं हूँ। परम सत्य की यदि कोई परिभाषा दी जा सकती है तो वही जो ईश्वर ने, परम सत्ता ने मोज़ेज को बतायी थी- "मैं जो हूँ, वही हूँ।" और जिन महापुरुषों ने भी धर्म की औपचारिकता को तोड़ते हुए इस अनुभव तक, इस रहस्यमयी अनुभूति के मर्म तक पहुँचने का प्रयत्न किया, उन्होंने अन्ततः स्वयं को एक सामान्य धरातल पर ही पाया, जहाँ सभी को वही शाश्वत अनुभूति हुई और वे कह सके "मैं हूँ, मैं हूँ।"
प्रागैतिहासिक काल में हजारों वर्ष पूर्व इस देश के रहस्यदर्शी और ऋषि जब इस अनुभव को उपलब्ध हुए, तब उन्होंने भी घोषित किया - "सत्य एक है; परन्तु अनेक नामों से पुकारा जाता है- 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति'।" वह गुह्य सत्य, वह शाश्वत सत्य केवल एक है, अनेक नहीं। वह अद्वैत है; क्योंकि असीम है, और जो-कुछ है सब वही है। इसीलिए कहा गया है- "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म।" वह परम सत्य ब्रहा है।
'ब्रह्म' से हिन्दुओं के त्रिदेवों में से प्रथम देव सर्जक क्रिया अथवा सर्जक-तत्त्व ब्रह्मा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वेदान्तिक भाषा में 'ब्रह्मन्' अथवा 'ब्रह्म' उसे कहा गया है जो जब कुछ भी नहीं था, तब भी था। वह नाम-रूप के प्रकट होने से पूर्व था, यहाँ तक कि सृष्टि से पूर्व था। वह 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' अजात है, कारण-रहित है, परन्तु समस्त पदार्थों का आदि कारण है। वह एक है, अद्वैत है, अतः आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, वह एक से अधिक नहीं हो सकता। आप उसे सर्वशक्तिमान् कहें, फादर इन हेवेन कहें, जेहोवा कहें, अल्लाह कहें, अहुरमज़दा कहें, ईश्वर कहें, निर्वाण कहें, महान् ताओ कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे इसे एक से अधिक नहीं बना सकते। वह आत्यन्तिक अद्वैत सभी धर्मों का भगवान् सब धर्मों से परे है। केवल वही नित्य है, अनन्त है, पूर्ण है और सम्पूर्ण है। जब तक मानवात्मा उस परम सत्ता के महा-अनुभव में प्रवेश नहीं करती, तब तक असन्तुष्ट और अतृप्त रहती है। जब तक मनुष्य पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक अपर्याप्तता का भाव उसके हृदय को, उसकी आत्मा को विदीर्ण करता रहता है।
जैसा कि हम जानते हैं, यह संसार खण्ड है, सीमित है, देश-काल-परिच्छिन्न है। यहाँ सब पदार्थ परिवर्तनशील हैं जो शीघ्र चले जाने वाले हैं। काल में ही उनका आदि और काल में ही उनका अन्त है, अतः वे शीघ्र समाप्त हो जाने वाले, क्षणिक और अस्थिर हैं। इस छोटे से क्षणिक काल-सातत्य में भी उनमें हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, सदैव परिवर्तन हो रहा है। और चूंकि ये सब अविश्वसनीय, परिवर्तनशील, शीघ्र समाप्त हो जाने वाले हैं; अतः मानवात्मा उनसे सन्तुष्ट नहीं हो सकती। उसे तो उसकी प्यास है जो पूर्ण है, अभाव-रहित है, शाश्वत, स्थायी और नित्य है। इस प्रपंचात्मक विश्व की किसी वस्तु से उसकी तृषा शान्त नहीं हो सकती। उसकी वह तृषा, वह क्षुध उस पूर्ण, अखण्ड और नित्य जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसके अतिरिक्त और किसी से शान्त नहीं हो सकती।
ईश्वर ही मानव की खोज है। वही समस्त धर्मों का लक्ष्य है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने देखा कि मानव-समाज सभी धर्मों के हृदय में निहित इस मूलभूत सार्वभौम तत्त्व को ग्रहण करने की चेष्टा करने और तात्त्विक एकता; जो मनुष्य को तत्काल आत्मीय रूप से पूर्ण बना कर विश्व में परस्पर एक-दूसरे के साथ आत्मीयता का भाव, सहयोग का भाव और ईश्वर की इस खोज में समभागी हो जाने का भाव-बोध जगाती है-ऐसी एकता की चेतना में प्रवेश करने की अपेक्षा वह एक ऐसी अवस्था में प्रविष्ट हो रहा है जहाँ सुगठित धर्म के बाहरी ढाँचे में लिप्त हो गया और पारस्परिक मतभेदों पर बल देना आरम्भ कर दिया। धर्म अपेक्षाकृत वैर, शत्रुता, फूट, तिरस्कार जैसी भावनाओं को पैदा करने का कारण बन गया।
वे इस बात से अत्यन्त दुःखी थे कि मनुष्य परस्पर उन्हीं वस्तुओं के लिए लड़ रहा है जो वस्तुएँ एकता लाने का कारण रही हैं। अतः गुरुदेव ने अपना जीवन-ध्येय बनाया इस अशान्त, व्यग्र बीसवीं शती के मनुष्यों में परस्पर एकता की भावना और मानवीय प्रेम उत्पन्न करना। धर्म एक है। ईश्वर एक है। धर्म की वास्तविक भाषा प्रेम की भाषा है। यह धर्म हृदय का धर्म है। आप जितना ही अधिक विभक्त हो कर जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे में परस्पर कितना अन्तर है, धर्म आपको दूसरों से उतना ही दूर ले जायेगा। इसके विपरीत आप धर्म के मर्म में छिपी इस सुन्दर एकता को जितना ही अनुभव करेंगे, उतना ही आप एक-दूसरे के निकटतर आने लगेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, मनुष्य का पिता एक है। धर्म एक है-मनुष्य को प्रेम करना और उसकी सेवा करना तथा उस परम दिव्य की पूजा और खोज में जीवनार्पण कर देना। उन्होंने भगवान् की पूजा करने को, उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करने को, समस्त जीवों को प्रेम करने और उनकी सेवा करने को कहा। संक्षेप में धर्म का हृदय यही दो चीजें हैं और ये ही समस्त धर्मों का अमर सन्देश हैं।
अरे मानव! उस परम की उपासना कर, सजग हो कर उसकी ओर बढ़ तथा ब्रह्मानुभव के लिए जागरूक हो कर प्रयत्न कर। सबको प्रेम कर। जीवन को अविराम सेवा, प्रेममयी सेवा और भ्रातृ-भावना का क्षेत्र बना ले।
उनकी सेवा की परिभाषा थी प्रेम की अभिव्यक्ति। प्रेम का अभिव्यक्तिकरण सेवा है। उनकी धर्म की परिभाषा थी भगवत्पूजा, इस अनुभव को उपलब्ध करने का सजग प्रयत्न।
यहाँ हम लोग अध्यात्म-विद्या (Theology) की शिक्षा-शाला में एकत्र है। अध्यात्म-विद्या ईश्वर-ज्ञान है। ईश्वर-ज्ञान हम धर्मशास्त्र पढ़ कर पा सकते हैं; सन्तों के सान्निध्य में, उनके पावन चरणों में बैठ कर, उनसे प्रश्न पूछ कर, उनके द्वारा दिये गये उत्तरों से, उनके द्वारा प्रदत्त प्रकाश से हम ईश्वर-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान हम उनसे ही पा सकते हैं जिन्हें उसके स्वरूप का ज्ञान है और जो उसे शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ईश्वर के इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मन, बुद्धि और विवेक द्वारा प्राप्त होता है। इसके द्वारा हममें दूसरों को ज्ञान बताने की क्षमता आ जाती है; परन्तु यह ईश्वर का जीवन्त अनुभव नहीं दे सकता। इसीलिए इस ज्ञान को 'परोक्ष' कहा जाता है।
परन्तु ईश्वर का दूसरा ज्ञान भी होता है जो ईश्वर के सम्बन्ध में गहरा, व्यक्तिगत, हमारी आध्यात्मिक प्रकृति की गहराइयों में छिपा अनुभव है। यहाँ न तर्क करने की कुछ गुंजाइश है, न सुनने की और न आश्वस्त होने की। यहाँ तो आप तत्काल ही पकड़ाई में आ कर चेतना के उस तल पर ले जाये जाते हैं जहाँ ईश्वर आपके लिए यथार्थ सत्य बन जाता है। जहाँ जगत्-बोध नहीं रह जाता, किसी का बोध भी नहीं रह जाता। यदि रहता है तो आपकी चेतना की गहराइयों में केवल दीप्त स्पन्दित प्रत्यक्ष भागवत अनुभव। यह अनुभव ईश्वर की असत्ता के संशय को सदा के लिए दूर कर देता है और ईश्वर का ज्ञान हर तरह से आपके लिए नितान्त निश्चित और विवाद-रहित उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार हथेली पर रखा हुआ फल। यह ज्ञान किसी प्रकार की इन्द्रियों से; चाहे वे भौतिक स्थूल इन्द्रियाँ हों या मन और बुद्धि जैसी सूक्ष्म इन्द्रियाँ हों; प्राप्त नहीं हो सकता। यह तो प्रत्यक्ष है, अनन्तरित है, आत्मिक है। इसे 'अपरोक्ष-अनुभूति' कहते हैं।
एक बार इस ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर आप वही व्यक्ति नहीं रह जाते। आप पूर्णतः रूपान्तरित हो जाते हैं। आपकी चेतना शुभ्र गुणों से उद्भासित हो उठती है जहाँ प्रत्येक पदार्थ दिन के प्रकाश की भाँति स्पष्ट हो जाता है। भगवान् आपके लिए एक जीवन्त तथ्य, आपके जीवन का, आपकी सहज चेतना का एक अंग बन जाता है। तभी आप कह सकेंगे कि आपका जीवन, आपकी गति तथा सत्ता भगवान् में है। यह ज्ञान ही उपलब्ध करने योग्य सारभूत वस्तु है। इसे 'अपरोक्ष-अनुभूति' कहते हैं। यह ज्ञान उतना ही नहीं है, जितना जीवन्त अनुभव है।
जिस प्रकार किसी व्यक्ति को निश्चित दिन तक चीनी के बारे में कि चीनी ऐसी होती है, इस विधि से चीनी बनती है, इस रूप-रंग की होती है, देखने में ऐसी लगती है तथा उसकी रासायनिक संरचना-वह सफेद चूरा है, डलियों (Cubes) के रूप में बिकती है, मिश्री के रूप में भी बिकती है, आदि-आदि सैकड़ों बातें बतायी गयी हों तो उस व्यक्ति को चीनी के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह चीनी के विषय में अच्छा खासा व्याख्यान दे सकता है, लेख लिख सकता है; परन्तु जब तक वह चीनी को चखता नहीं, जीभ पर रख कर उसकी मधुरता का आस्वादन नहीं करता तब तक चीनी विषयक वास्तविक और श्रवण किये हुए ज्ञान में बड़ा अन्तर रहेगा। अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान में भी यही अन्तर है।
ब्रह्मानुभव में प्रवेश कीजिए और इसे अपना जीवन्त अनुभव बनाइए। यह आवश्यक है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पुनीत शिक्षा-संस्था के अध्यात्म-ज्ञान के समस्त छात्र ईश्वर, संसार, मनुष्य के विषय में तथा मनुष्य और संसार के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में व्याख्यानों, पुस्तकीय अध्ययन और चिन्तन द्वारा ज्ञान ग्रहण कर स्वयं को सम्पन्न तो बनायें ही, साथ-ही-साथ मेरी हार्दिक कामना है कि अपने हृदय में, अपने अन्तरतम में भगवान् के जीवन्त अनुभव की खोज भी निरन्तर जारी रखें।
मेरे आत्मीय बन्धुओ! मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूँ कि अध्यात्म- विद्या जो आप यहाँ सीख रहे हैं, वह स्वयं अपने में ध्येय नहीं है-आप इसे भी जानें। यह किसी सांसारिक प्रयोजन, काम-धन्धे की पूर्ति का साधन भी नहीं है कि यह आपको पादरी बनने की क्षमता दे दे या इस ज्ञान से आप अध्यात्म-विद्या के लेखक बन जायें या चर्च के मूल-सिद्धान्तों का जन-समूह में प्रचार करने वाले प्रचारक बन जायें-इतना भी नहीं। यह ज्ञान इसका भी साधन नहीं है। परन्तु आपको अपने अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए और अपनी थियोलोजी को ईश्वर के जीवन्त अनुभव में प्रवेश करने का साधन बनायें। वही अध्यात्म-विद्या का मूल-तत्त्व और प्रतिपाद्य है।
मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जिस जिन आपको भगवान् के महा-अनुभव का वरदान मिलेगा, जिस दिन आप उस परमात्मा से युक्त हो कर आत्मा की अन्तज्योंति से ज्योतिर्मय बन जायेंगे। इसी मिलन से जीवन परिपूर्ण होता है; अस्तित्व में औचित्य आता है। केवल इसी के द्वारा आप उस आत्मिक चैतन्य की अवस्था को उपलब्ध होंगे जिसमें फ्रांस के सन्त जान, अविल की सन्त टेरेसा और असीसी के सन्त फ्रांसिस जैसे महान् रहस्यवादियों की तरह आप कह सकेंगे- "मैं परम पिता परमेश्वर का बालक हूँ, केवल वे ही मेरे पिता हैं। मैं यहाँ का नहीं हूँ, उस परम पिता का हूँ।" ये सब ईश्वर-अनुभव में उतरे हुए ईसाई धर्म के प्रकाश-पुंज हैं।
प्रिय बन्धुओ! अपनी इस अध्यात्म-विद्या को परम अनुभव में जाने की आधारशिला बना लो। किसी भी अन्य चीज से सन्तुष्ट न होना। केवल उसे ही लक्ष्य में रखो। गिरजे का एक विनम्र सेवक बन कर, ईश्वर के सन्देश का प्रचार करने के साथ-ही-साथ परिपूर्ण गतिशील, नितान्त आध्यात्मिक आन्तरिक जीवन यापन करते रहो। ऐसा करने पर ही हम दिन-प्रति-दिन उत्तरोत्तर ईश्वर-चेतना के महानुभाव के निकट से निकटतर होते जायेंगे। इसी परम अनुभव को निर्विकल्प समाधि कहा गया है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का प्रमुख जीवन-ध्येय यही था। वे इस दिखायी देने वाले नानात्व से हमारा ध्यान हटा कर परम अनुभव को लाना चाहते थे।
इसके साथ ही बीसवीं सदी की मानवता के हितार्थ उन्होंने जो अमूल्य सेवा-कार्य किया, वह है आज की मानवता को आध्यात्मिक जीवन की ओर, आध्यात्मिक गुणों की ओर तथा आध्यात्मिक खोज की ओर पुनः ले आना। इसके बिना समस्त धर्म और उनकी साधनाएँ केवल औपचारिक ही हैं। और वह हिन्दू भी केवल औपचारिक हिन्दू है जो हिन्दू-जीवन के बाहरी कलेवर की पूर्ति करता है और अन्तर से वह बिलकुल खोखला, ईश्वर को जानने की आकांक्षा से रहित, निपट दिवालिया है। ईश्वर के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। केवल अपने लिए सन्तोष चाहता है कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, अधार्मिक नहीं हूँ। अधर्मी होने का दोष न लग जाये, इस कारण वे धर्म के बाहरी स्वरूप की पूर्ति करते रहते हैं। आज के मुसलमान केवल नाम के मुसलमान रह गये हैं। ईसाई भी केवल नाम के ईसाई हैं। पारसी भी केवल नाम के पारसी हैं।
लगभग अट्ठानवे, निनानवे प्रतिशत मनुष्य अपने धर्म या सम्प्रदाय से केवल मौखिक नाता जोड़ते हैं। वे धर्म के केवल बाहरी रूपों तक हैं, जब कि धर्म-स्थापना का वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य को ईश्वर की खोज की प्रेरणा देना, ईश्वर का अनुभव देना। यह लक्ष्य पता नहीं कहाँ खो गया है और धर्म अध्यात्म-विहीन हो गया है, शुष्क हो गया है। गुरुदेव आये और जीवन पर्यन्त यथाशक्ति धर्म की इस आध्यात्मिक रिक्तता को पूरी करने में लगे रहे। अतः धर्म का अर्थ हमारे लिए है ईश्वर को जानने का सजग प्रयास, अभी इसी क्षण ईश्वरानुभव में प्रविष्ट हो जाने का प्रयास। अत धर्म को, ईश्वराभिमुख अप्रतिहत गति, आध्यात्मिक प्रक्रिया से स्पन्दित गति होना चाहिए। केवल बहिर्मुखी कार्यावलि होने से काम नहीं चलेगा।
अतः वे चाहते थे कि धर्म आपकी अन्तर की गहराइयों में प्रवेश कर जाये और आपके हृदय के अन्तरतम में सक्रिय हो उठे। इसीलिए उन्होंने यह महान् सन्देश दिया-"जीवन का ध्येय आत्म-साक्षात्कार है।"
अरे मानव! उठ खड़ा हो। जीवन एक अद्भुत अवसर के रूप में तुम्हें मिला है। इस अवसर से लाभ उठाओ और ईश्वर को उपलब्ध हो जाओ। इस शरीर के पतन से पूर्व, इस भौतिक देह के अन्त से पहले ही किसी भी तरह ईश्वरानुभव प्राप्त कर धन्य हो जाओ। जीवन को सफल बनाओ। यही एक चीज है जो वास्तविक सफलता से, ईश्वर के प्रत्यक्ष जीवन्त अनुभव से तुम्हारे जीवन को महार्घता देती है। इसलिए मानव की निःस्वार्थ सेवा द्वारा, सबमें ईश्वर के दर्शन द्वारा इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करो। अपने दैनिक कार्यों के मध्य में भी ईश्वर को अनवरत याद करो। जो-कुछ करो, सब उससे ही युक्त कर दो।
प्रत्येक कर्म, चाहे वह कितना ही छोटा, साधारण, क्षुद्र, महत्त्वहीन क्यों न प्रतीत होता हो, वह महत्त्वहीन नहीं है। उसे भगवान् से जोड़ दो। जो हर क्रिया को ईश्वर से जोड़ता है, उसे विश्व-नाटक के इस सांसारिक अभिनय में बँधा न समझो। उस ईश्वर से कहो- "हे भगवन्! मनसा, वाचा और कर्मणा मैं जो कुछ भी करता हूँ, आपके चरणों में समर्पित है। इस प्रकार मैं तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ। मेरा छोटे-से-छोटा कर्म, चाहे वह घर में, बाजार में, समाज में, व्यवसाय में, कहीं भी क्यों न किया गया हो, सब तुम्हें अर्पित करता हूँ। तुम्हारे प्रेम में ही मैं यह करता हूँ और तुम्हें ही अर्पित है।"
इस प्रकार उन्होंने कहा कि अपनी सांसारिक क्रियाओं को ऐसी क्रियाओं में बदल डालो जो तुम्हें सीधे ईश्वर से जोड़ती हैं। सब प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करो। वह केवल अतीन्द्रिय, अभौतिक सत्य नहीं है, प्रत्यक्ष और आन्तर सत्य भी है। वह सर्वत्र है, इस क्षण भी यहाँ है। अतः उसे सर्वत्र देखो और अपने समस्त कर्म परम श्रद्धापूर्वक उसे ही अर्पित करो। अपना समस्त जीवन ही उसको अर्पित कर दो और इस प्रकार अपने जीवन को स्वतः ही प्रभु की ओर अनवरत गतिशील प्रक्रिया बन जाने दो। कर्म श्रद्धा है। जीना प्रार्थना है। कर्म सचमुच में नित्य विद्यमान दिव्य की उपासना है।
इस प्रकार उन्होंने हमारे सम्पूर्ण जीवन के प्रत्येक क्षण को दिव्य बनाने का सन्देश दिया। प्रातःकाल से रात्रि पर्यन्त आप और कुछ नहीं, केवल भगवान् की पूजा-उपासना करते हैं। उसी के पुजारी हैं। गिरजे, सिनागोग, मन्दिर, मसजिद या गुरुद्वारे ही मात्र पूजा-स्थल नहीं हैं, वरन् आप जहाँ-कहीं भी पूजा-भाव से हैं वहीं वस्तुतः आप गिरजे में हैं, प्रभु के समक्ष हैं। अतः सभी स्थान पावन हैं, उसकी सत्ता से पवित्र हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि वह उस दिव्य को सौन्दर्य अर्पित करे।
जैसे यह सुन्दर-सी पुष्पमाला मुझे पहनायी गयी है, वैसे ही आप सम्पूर्ण जीवन को परम सत् परमेश्वर के लिए, उस भगवान् के लिए जो सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, माला बना लें और अपने प्रत्येक कार्य को उस माला में गूँथा जाने वाला पुष्प। आपका हर कार्य उस जीवन-माला का सुमन बन जाये जिस माला को आप भगवान् को अर्पित करने जा रहे हैं। अतएव अपनी क्रियाओं को आध्यात्मिक बना लें, उन्हें योग-कर्म में रूपान्तरित कर लें। उसकी अदृश्य सत्ता का हर समय अनुभव करें। उसे अखिल सृष्टि में ओत-प्रोत और समस्त नाम और रूपों में वास करने वाले के रूप में देखें तथा इस प्रकार अपने जीवन को ईश्वर-अनुभव की ओर उत्तरोत्तर गतिशील एक महान् प्रक्रिया, सम्पूर्ण प्रक्रिया बना लें। मनुष्य मात्र से प्रेम करें। ईश्वर की उपासना करें। उसका अविराम स्मरण करें। समस्त कार्यों के मध्य भी उसका चिन्तन करें।
प्रातः और सायं कुछ समय निकाल कर अपनी आत्मा में प्रवेश करें। बहिर्गत को भूल जायें। शरीर को भूल जायें। समय को भूल जायें और आत्मा में चले जायें तथा सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान् के समीप शान्त और स्थिर रूप से टिक जायें। चिन्तन करो, ईश्वर का ध्यान करो और अपने जीवन को प्रफुल्लित करके अपनी आध्यात्मिकता को पुनः शक्ति-सम्पन्न करो। तदुपरान्त अपने दैनिक कार्य में लग जाओ। रात्रि में एक बार पुनः भगवान् में उतरो। इस प्रकार आत्म-साक्षात्कार करो। सबकी सेवा करो। उस परमेश्वर की प्रतिदिन उपासना करो। उपासना नियमित रूप से गहरे ध्यान के रूप में करो और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उसकी खोज जारी रखो। उसे आत्मिक रूप में उपलब्ध करो। सेवा, प्रेम, ध्यान और साक्षात्कार करो।
आपमें अध्यात्म के आवश्यक अपरिहार्य गुण प्रतिष्ठित करने वाले दिव्य जीवन के सन्देश के लिए हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का जीवन समर्पित था। उन्होंने सार्वभौम आध्यात्मिक सन्देश दिया। उन्होंने किसी विशेष 'धर्म' या 'वाद' का प्रचार नहीं किया, प्रत्युत आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक खोज के सन्देश को प्रसारित किया, जिसके बिना धर्म वास्तविक जीवन से शून्य हो जाता है, शुष्क हो जाता है, तत्त्वहीन हो जाता है।
अतः मेरे प्रिय बन्धुओ! धर्म का सार है ईश्वर की खोज और उसका अनुभव। आपकी यह अध्यात्म-विद्या ईश्वर का जीवन्त व्यक्तिगत अनुभव-प्राप्ति में, ईश्वर का वास्तविक आन्तरिक ज्ञान प्राप्त करने में सजीव स्पन्दनशील प्रक्रिया बन जाये। साधारण अर्थ में ईश्वर का ज्ञान इसका आधार है। ईश्वर-ज्ञान के इस आधार पर, इस नींव पर ही ईश्वरानुभव का भवन निर्माण करो और कृतार्थ हो जाओ। आपका जीवन महान् अनुभवों से मण्डित हो ! यह शरीर छूटे, उससे पूर्व ही आप इस ईश्वर-चेतना में संस्थित हो जायें-उसी चेतना की भूमिका पर जिस पर स्वयं ईसा मसीह थे और जानते थे कि वे परमात्मा के पुत्र हैं। उनका वह कथन कथन मात्र नहीं था। वे परमात्मा के पुत्र हैं, इसे वे अपनी अन्तरतम सत्ता में जानते थे। आप सब उस चेतना को प्राप्त हों जिससे यह कह सकें-"मैं परम पिता का पुत्र हूँ।" और इस तरह अपने को परम धन्य बनायें।
अपने लिए प्रकाश बन जाओ। समस्त प्राणियों के लिए प्रकाश बन जाओ। परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरी यही विनम्र प्रार्थना है तथा आपमें से प्रत्येक से मेरा यही हार्दिक अनुरोध भी है। भगवान् को ढूँढ़ने और पाने के लिए ही जीओ। मानव के प्रति और भगवान् के प्रति जो प्रेम-भाव है, उसे सबको समाहित करने वाली प्रेम की ऐसी महान् भावना में परिणत कर लो जो आपको स्वयं को भुलवा दे तथा हर एक के लिए आनन्द, उल्लास, सान्त्वना, सेवा, सहायता प्रदान करने का केन्द्र बन जायें। आपका जीवन आदर्श बन जाये। आपका जीवन ब्रह्मानुभव में पूर्णत्व प्राप्त करे! आप सभी पर सदैव भगवान् की कृपा हो! सभी पूर्व-पश्चिम के सन्तों के, प्राचीन-अर्वाचीन सन्तों के, विगत और वर्तमान सन्तों के आशीर्वाद आप पर हों! इस सेवक की प्रार्थना भी सदा आपके साथ होगी। भगवान् करे, आपका जीवन आध्यात्मिक गुणों से प्रकाशित हो, प्रभु-प्रेम से आपका जीवन स्पन्दित हो जाये, आप प्रभु की खोज की लगन से भरपूर हो जायें और ईश्वर-साक्षात्कार से आपका जीवन आलोकित और प्रकाशित हो जाये!
२३.मानव-जीवन का लक्ष्य
इस संसार में तीन वस्तुएँ दुर्लभ हैं-मानव-जन्म, मोक्ष की कामना और सन्तों का संग। ये तीनों भगवत्कृपा और उसके अनुग्रह से प्राप्त होती हैं। इन तीनों में मनुष्य-जन्म अमूल्य वरदान है; अतः उसे प्रथम स्थान दिया गया है। सत्ता की यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीव को बुद्धि और नित्यानित्य-वस्तु-विवेक की अति-दुर्लभ क्षमता उपलब्ध होती है। इसीलिए मनुष्य-जीवन भगवान् की अत्यन्त दुर्लभ देन माना गया है। अतः मनुष्य-जीवन प्राप्त करके भी यदि आपमें उस अवस्था को पहुँचने की तीव्र अभिलाषा नहीं है जो आपको नित्य आनन्द और अमरता प्रदान करेगी, तो इसका अर्थ है कि आप इस मनुष्य-जीवन का उपयोग किसी लक्ष्य हेतु नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा ही है, तो आपका अस्तित्व पशुवत् है। खाना, पीना, सोना और वासना-जन्य आनन्दोपभोग मनुष्य और पशु में समान हैं। मनुष्य का आदर्शवाद और भौतिक सत्ता से कहीं ऊपर उठने की उसकी आकांक्षा उसे पशु से भिन्न बना देती है। हम जानते हैं कि हमें कुछ उच्चतर प्राप्त करना है तथा इस भौतिक जीवन की अपूर्णताओं से मुक्त होने की तीव्र आकांक्षा भी हममें है।
इसके पश्चात् आता है विद्वज्जनों का संग। उक्त दो वस्तुएँ अर्थात् मानव-जन्म और मुमुक्षुत्व प्राप्त कर लेने पर भी हमारा जीवन भ्रम से आवृत रहता है, असफल प्रयासों से भरा रहता है। यह सब केवल इसी कारण कि हम नहीं जानते कि सही प्रयत्न क्या है? सम्यक् प्रयत्न की क्षमता तो उस भाग्यशाली व्यक्ति को प्रदान की गयी है जिसे पथ की बाधाएँ दूर करने वाला यह तीसरा वरदान प्राप्त है। यदि हम स्वयं को प्रभु को अर्पित कर दें, तो वह हमें मार्ग दिखाता है। जब प्रलोभन हमें पथ-भ्रान्त करता है, उन क्षों में वह हमें प्रेरणा दे सकता है, उत्साह और साहस दे सकता है। हमें तीनों ही वरदान प्राप्त हैं-तीनों ही नहीं, प्रत्युत चारों अर्थात् मन भी। मन भी सहमति जतायेगा। मानव-मन से बड़ा कोई दानव नहीं है। वह माया का दूत है; अत: ईश्वर-प्राप्ति के माम में बाधक है। अतएव मन अनुकूल होना चाहिए। आप पर चाहे देव-कृपा हो गुरु-कृपा और शास्त्र-कृपा ही क्यों न हो, मन को आपका सहयोगी होना ही चाहिए।
हम अपने परम ध्येय, परमादर्श की ओर दिन-प्रति-दिन उन्नति तथा प्रगति करते जाने के लिए ही यहाँ हैं। अतः आज का यह शुभ दिन और पुनीत अवसर है कि आज से हम ऐसी नियमित कक्षाएँ चालू कर रहे हैं जिनमें ध्यान के सिद्धान्त बताये जायेंगे, ध्यान का अभ्यास कराया जायेगा तथा साधना के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए यह भी बताया जायेगा कि अपनी प्रत्येक क्रिया को आध्यात्मिक किस प्रकार बनाया जाये। हम प्रातः और सायं ध्यान करते हैं; परन्तु फिर भी दिन-भर के अपने कार्य-व्यापार तथा अन्य के संग व्यवहार में अति-संकीर्णता और स्वार्थपरता दिखाते हैं। यह हमारी साधना में अवरोध पैदा कर ध्यान के परिणाम को नष्ट कर देते हैं।
यूलिसिस की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी पेनेलोप के कई चाहने वाले हो गये; परन्तु वह किसी दूसरे की पत्नी होना ही नहीं चाहती थी। वह निष्ठावान् और पतिपरायण स्त्री थी। अतः उसने अपने प्रणयियों से कहा कि वह एक वस्त्र बुन रही है और जब तक वह वस्त्र तैयार नहीं हो जायेगा, वह तब तक किसी से विवाह नहीं कर सकती। उन्होंने मान लिया और जब तक यूलिसिस लौट कर नहीं आया, वह दिन-भर वस्त्र बुनती रहती और दिन-भर का बुना रात में उधेड़ देती। इसी तरह का उधेड़ना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रातः और सायं हमने जितनी भी साधना की हो, उसमें हमें अदिव्य तत्त्व नहीं जोड़ने चाहिए।
अपने कार्यों के बीच में यदि हम अपने मूलभूत तत्त्व को भूल जाते हैं, रुक्ष हो जाते हैं, किसी की आलोचना करते हैं या सच्चाई से हट जाते हैं, तो जो साधना हमने ध्यान के क्षणों में की है, उसे उधेड़ कर रख देते हैं। अतः हमारा बहिर्गत जीवन और हमारी क्रियाएँ, हमारी वाणी और कर्म, हमारे ध्यान, उपासना और साधना की भावना के अनुरूप हों और उस भावना का संवर्धन करने वाले हों। इसलिए अपनी साधना को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि उसे हम केवल अपने शान्तिपूर्ण क्षणों तक ही सीमित न रख कर अपने समस्त कर्मों में दिव्यता ले आयें। हमारे समस्त कर्म हमारे वास्तविक स्वभाव के अभिव्यंजक हों। वे दिव्य हो जायें।
यही कारण है कि कर्मयोग में समस्त कर्मों को दिव्यता प्रदान की जाती है। यह सबको जानना चाहिए-चाहे वह ध्यानयोगी हो, भक्त हो या वेदान्ती हो। कर्मयोग बड़ा कठिन है। एकान्त में आपकी बड़ी आदर्श भावना हो सकती है; परन्तु कठोर यथार्थ से सामना होने पर, इस विषमताओं से भरे जगत् में सन्तुलन रखना, केवल दिव्यता को अभिव्यक्त करना तथा निःस्वार्थ रहना बड़ा कठिन कार्य है। परन्तु फिर भी स्पृहणीय है; क्योंकि इसके द्वारा अन्य योग सफल हो जायेंगे।
जो मनुष्य आत्म-त्याग की भावना के साथ, माधुर्य के साथ आदर्श जीवन व्यतीत करता है, उसका एक माला जप भी अन्य व्यक्तियों की हजारों माला जप के बराबर होता है; क्योंकि उसका स्वभाव दिव्य कर्मों के द्वारा पवित्र और समुद्यत हो जाता है। परन्तु यदि स्वभाव काम, क्रोध आदि से पूर्ण है तब चाहे आप ध्यानोपासना करते रहें, पर भूमि तैयार न होने से वह फलवती नहीं होगी।
व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि उसकी उन्नति क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो रही है; क्योंकि अपने कार्यरत जीवन में वह साधना के प्रतिकूल चलता है। साधक को विवेकशील होना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि छिद्र कहाँ है? अन्यथा पात्र टपकता ही रहेगा। आप कितना ही भरते जायें, व्यर्थ है। अतः आपको जानना होगा कि पात्र कहाँ से रिसता है और इस हेतु आपको कर्मयोग की कला का ज्ञान होना चाहिए।
इसका व्यावहारिक ज्ञान आपको आश्रम की कक्षाओं में ही मिलेगा। एक राजा के पास तीन खोपड़ियाँ थीं। उसने अपने राज-पण्डित से पूछा कि इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है? उस पण्डित ने एक खोपड़ी को लिया और उसके कान में तार डाला। वह तार दूसरे कान से बाहर निकल आया। दूसरी खोपड़ी के कान में जब तार डाला गया, तो वह मुख-द्वार से बाहर आ गया। तीसरी खोपड़ी के कान में जब तार डाला गया, तो वह सीधा वक्ष में चला गया। राज-पण्डित ने बताया कि तीसरी खोपड़ी श्रेष्ठ है।
पहली खोपड़ी ऐसे लोगों की प्रतीक है जो एक कान से सुन कर उसे आत्मसात् किये बिना ही दूसरे कान से निकाल देते हैं और उसके विषय में भूल जाते हैं। दूसरी खोपड़ी उन लोगों की प्रतीक है जो ज्ञान प्राप्त कर उसे जनता में फैलाने को तो व्यग्र रहते हैं, परन्तु स्वयं उस पर नहीं चलते। ये द्वितीय श्रेणी के लोग हैं। तीसरी खोपड़ी श्रेष्ठ कोटि के साधकों की प्रतीक है जो ज्ञान श्रवण कर उसे हृदयंगम कर लेते हैं और उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करने की चेष्टा करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप तीसरी खोपड़ी की तरह बन जायें और जो कुछ भी बुद्ध जनों के संग से, सन्तों और महात्माओं के निकट सत्संग से प्राप्त हो, उसका विकास और अभ्यास करें। भगवान् का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो!
२४.समृद्धि का विधान
आयुर्वेद का सिद्धान्त कहता है कि व्याधि का मूल शरीर नहीं है, मन है। यह व्याधि ही सब भौतिक रोगों का कारण है; अतः इसका व्याधि नाम बड़ा अर्थपूर्ण और सार्थक है। शारीरिक रोगों को उन्होंने व्याधि कहा है और इन शारीरिक व्याधियों के मूल को, मानसिक कारण को 'आधि' कहा है। पहले एक रोग आता है, तब दूसरा उसी से पैदा होता है। तदनन्तर उसका परिणाम प्राण-शक्ति के दुरुपयोग के कारण प्रकट होता है। प्राणिक ऊर्जा के दुरुपयोग से शरीर में कुछ ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है जो बीमारी पैदा कर देती है।
भारत के प्राचीन ऋषियों ने शरीर की दशाओं की अद्भुत प्रकार से व्याख्या की है; पाश्चात्य ढंग से नहीं की है। मन के मल के कारण जो अवस्थाएँ प्रकट होती हैं, उन रुग्ण अवस्थाओं के निदान के लिए आयुर्वेद में एक सिद्धान्त 'त्रिदोष' का था। आपकी प्राण-शक्ति शरीर के 'त्रिदोष' पर निर्भर है। वे कहते हैं कि मन की शुद्धता और प्राण-शक्ति की सूक्ष्मता में किसी प्रकार गड़बड़ हो जाने से, मानव मात्र की सामान्य अवस्था का निर्माण करने वाले इन त्रिदोषों में असन्तुलन आ जाता है। मध्ययुगीय यूरोप और इंग्लैण्ड में औषधि-क्षेत्र में 'त्रिदोष' का सिद्धान्त अनजाना नहीं था। मेरा विश्वास है कि यूरोप की पद्धति कुछ-कुछ आयुर्वेद जैसी ही थी और सम्भवतः वह अरब और यूनान के माध्यम से आयी थी।
ये तीन दोष-कफ, पित्त और वात हैं। सामान्यतः स्वस्थ शरीर में ये सब एक विशेष मात्रा में पाये जाते हैं और जब प्राण-शक्ति के कुप्रयोग अथवा दुरुपयोग के कारण, आसक्ति के कारण किसी प्रकार की अनियमितता उत्पन्न हो जाती है या गलत चिन्तन और भावनाओं के कारण मन में गड़बड़ी हो जाती है, तब तीनों दोषों में असन्तुलन आ जाता है; परिणामतः रुग्णता की स्थितियाँ प्रकट होने लगती हैं। इस असन्तुलन के कारण यदि कफ का जोर हुआ तो कफ-सम्बन्धी बीमारियाँ यथा खाँसी, फेफड़ों में कष्ट, सरदी, जुकाम आदि आ घेरती हैं और यदि यह असन्तुलन अधिक वायु के कारण होता है तो सन्धिवात, उदरस्फीति, कटि-वेदना आदि प्रकट हो जाते हैं।
आयुर्वेदिक चिकित्सक त्रिदोषों में उत्पन्न विषमता को दूर करने के लिए ही औषधि देता है; परन्तु यह भी कहता है कि इस औषधि द्वारा मैं आपके त्रिदोषों को एक बार पुनः सम करने का प्रयास तो करूंगा; परन्तु भीतर से आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अतः सबसे पहली आवश्यकता है पूर्ण आत्म-संयम की। इसके बाद संवेग आते हैं। सभी बुरे संवेगों को त्याग दीजिए। परन्तु कैसे? यहाँ आयुर्वेदिक ऋषि बड़े सहायक रहे हैं। वे वह मनोविज्ञान नहीं जानते थे जिसका आधुनिक मनोवैज्ञानिकों को पता है; परन्तु फिर भी वे उस चीज को जानते थे जिसे जानना चाहिए था। उन्होंने कहा- "यदि आप मन को शान्त करना चाहते हैं और उसे संवेग-रहित बनाना चाहते हैं, तो उसमें अध्यात्म की तरंग उठाइए।" और इस उद्देश्य हेतु चिकित्सक सदैव किसी मन्त्र का जप करने को या किसी विशेष देवालय में जा कर किसी देवता- विशेष की किसी विशेष विधि द्वारा पूजा करने को कहता था।
जानते हो, पूजा एक ऐसा शक्ति-सम्पन्न साधन है कि एक बार भी यदि तुम अपने मन को ईश्वरोन्मुख कर लो, उसकी सत्ता को उस परम सत् से एक कर लो जिससे तुमने स्वयं को विच्छिन्न कर लिया है-यह विच्छिन्नता ही वास्तव में सांसारिक सत्ता या मानव-जन्म नामक महा-व्याधि का मूल कारण है-तो तुम्हारे मन में आमूल परिवर्तन आ जायेगा, एक बहुत बड़ा बदलाव आ जायेगा। पूजापरायणता में यदि तुम उस दिव्य से एक हो कर मन्त्र जपने लगो, दिव्य नाम का उच्चारण करने लगो, तो तुम्हारा मनस्तत्त्व शुद्ध और सूक्ष्म हो जायेगा तथा जिस स्थूल अवस्था ने भौतिक शरीर में रुग्णता के चिह्न पैदा किये थे, वह ठीक हो जायेगी। चिकित्सक बाहर से अन्तर की ओर तथा रोगी अन्तर से सहयोग करे, तो शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है। संक्षेप में, जिसे पंचम वेद भी कहते हैं, उस आयुर्वेद की यही पद्धति और प्रणाली है।
आयुर्वेद का प्रतिपाद्य है कि मनुष्य दिव्य है और स्वास्थ्य उसकी स्वाभाविक दशा है और शुद्धता तथा सूक्ष्मता उसकी पूर्वापेक्षाएँ हैं। इसलिए वह बड़ी रोचक घोषणा करता है। जीवन के प्रति हिन्दू-दृष्टिकोण है कि व्यक्ति चार पुरुषार्थों के निमित्त, चार महा-उपलब्धियों के हेतु जीवन यापन और कर्म करता है। वे हैं-धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। 'धर्म' नैतिक आदर्शों की पूर्ति है। 'अर्थ' सम्यक् जीवन यापन हेतु ईमानदारी से धनोपार्जन करना है। 'काम' उन विधानोक्त इच्छाओं की पूर्ति है जो ईमानदारी से, सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए, आत्म-कल्याण और जन-कल्याण के लिए आवश्यक होती हैं; उन सभी इच्छाओं की पूर्ति है जो दूसरों के कल्याण के विरुद्ध न हों। 'मोक्ष' है उस प्रभु को उपलब्ध हो जाना, उस परम दिव्य में नित्य मुक्त हो जाना।
आयुर्वेद का कहना है कि उक्त चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का स्वास्थ्य सर्वोत्तम मूल अथवा आधार है। स्वास्थ्य के बिना इनमें से कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता; अतः शरीर की उचित रूप में देखभाल भी प्रमुख कर्तव्यों में आती है और यह सन्तुलन और संयम द्वारा, सम्यक् चिन्तन, सम्यक् भावना और पूजा-भाव द्वारा मानसिक वृत्तियों में सम्यक् परिवर्तन ले आने से प्राण-शक्ति के संचय द्वारा होता है। उचित मात्रा में, उचित समय पर, उचित विधि से किया हुआ भोजन भी शारीरिक अवस्था को उचित दशा में रखता है; अतः ठीक समय पर, शान्त मन से भोजन खूब चबा कर करें और भोजन के उपरान्त थोड़ा विश्राम करें। सदैव परिमित रहने का प्रयत्न करें। भोजन सदैव पूजा-भाव से ग्रहण करें; क्योंकि भोजन ही जीवन-दाता है और भोजन ही जीवन हन्ता है। यह सब बहुत महत्त्वपूर्ण है।
यदि इस प्रकार स्वास्थ्य की देखभाल होने के कारण प्राणिक शक्ति के संचय और मन की सम्यक् वृत्ति के कारण आप स्वस्थ दशा में हैं-जीवन यापन की समुन्नत परिस्थिति भी आप प्राप्त कर लें, इसके लिए क्या यत्न करेंगे? समृद्धि का समुचित स्तर आपको कैसे प्राप्त हो सकेगा? समृद्धि का अर्थ लोभ और लालसा तथा अदम्य इच्छाओं की तृप्ति में न हो कर विधानोक्त सीमाओं के अन्तर्गत मन को शान्ति प्रदान करने वाले तथा मन की चिन्ता, विक्षेप और अशान्ति दूर करने वाले सरल जीवन में पाया जायेगा। सरल जीवन जो आपके मन में ऐसी भावना और ऐसे विचार दे सकेगा कि आप अपने साथियों की सेवा कर सकें तथा दत्तचित्त हो भगवान् की सेवा कर सकें और इस प्रकार बाहर का कल्याण, अपना परम कल्याण कर सकें।
समृद्धि के क्या सिद्धान्त हैं? मैं आपको समृद्ध होने का गुर नहीं बता रहा हूँ। मैं तो केवल उसके सिद्धान्त बता रहा हूँ। लेकिन समृद्धि का रहस्य भी अपनी आय की सीमा के भीतर ही रहना है-आय से कम खर्चे । ऋणग्रस्त कभी न रहिए। अति संक्षेप में, सबसे कीमिया बात यही है। तब समृद्धिशाली बना कैसे जाये ? यदि आप पाँच सौ रुपये कमाते हैं और चार सौ नब्बे खर्च करें, तो दस रुपये आपके पास हमेशा बचते रहेंगे। यदि आप इस विषय पर कुछ कहने की अनुमति दें तो मैं कहूँगा कि किश्तों पर कोई वस्तु न खरीदिए। किश्तों पर खरीदने की आदत न डालिए। नगद है तो खरीदिए; यदि नहीं है तो न खरीदिए। उसके बिना काम चला लीजिए।
तथापि कुछ तो समृद्धि के नियम हैं ही जो शाश्वत आध्यात्मिक सत्य से उद्भूत हैं। यदि आप अभाव का चिन्तन करते हैं और आपको अभाव लगता है, तो आपको अभाव का अनुभव होगा और यदि आपको अपने वैभव पर विश्वास है तो जिस प्रकार व्यक्ति की छाया उसका अनुसरण करती है, उसी प्रकार वैभव आपके पीछे चलेगा। यदि आप कुछ चाहते हैं, तो आप तत्काल अपना दरिद्र होना स्वीकार करते हैं। इच्छा दारिद्रय है। वह अपर्याप्तता का भाव है। आप ज्यों ही इच्छा करने लगते हैं, कुछ चाहने लगते हैं, चाहने से पूर्व ही याचक हो जाते हैं। समृद्ध होने का रहस्य है समृद्धि के इस सिद्धान्त के अनुरूप जीवन यापन करें। साथ ही अपनी सामान्य बुद्धि को, कामनसेन्स को काम में लायें।
एक बार वस्तुओं की इच्छा करने से यदि आपने दरिद्रता को दृढ़ करना आरम्भ कर दिया, तो दरिद्रता ही नियम बन जायेगी। इच्छा-रहित हो जाने में ही समृद्धि के विधान को सक्रिय कर देने का राज है। क्यों? क्योंकि आपके अन्तर में ही समस्त ऐश्वर्य है। कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी आपको कमी हो; क्योंकि आप भगवान् के हैं और भगवान् ही सब-कुछ है। सर्वेसर्वा वही है। वही सबका स्रोत है। उसी में सब-कुछ है। और जब आप जानेंगे कि आप उसी में हैं, तो आप सब पा लेंगे और आप सब हो जायेंगे। करना केवल इतना भर है कि इस तथ्य को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो कि आप सर्वदा उसी में हैं जो सर्वेसर्वा है। कुत्ता जैसे अपने स्वामी का अनुगामी होता है, उसी प्रकार समृद्धि को अपनी अनुगामिनी बना लेने की यही मुख्य कुंजी है।
आखिर को आप अखिल सृष्टि के स्वामी तो हैं ही; क्योंकि आप उसके उत्तराधिकारी हैं जो सभी का स्वामी है। आपको कोई कमी नहीं है। आप सर्वैश्वर्यमयी, वैभवमयी आत्मा हैं। आपका वास्तविक स्वरूप भूमा है, पूर्णत्व है। आप इस भावना को जितना ही दृढ़ करेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ इसे मानेंगे, मानना ही नहीं प्रत्युत पूर्ण आस्था के साथ मानेंगे-उतनी ही समृद्धि आपके लिए सुनिश्चित है।
अभाव और दरिद्रता की भावना मन की वृत्ति है। आपके पास जितना है, उसी में आप अनुभव करते हैं कि आपके पास सब-कुछ है, तब आपको कुछ नहीं चाहिए; परन्तु आपके पास सब-कुछ रहते हुए भी यदि आप सोचते हैं कि यह आपके पास नहीं है, तो आपके पास कुछ अतिरिक्त होगा ही नहीं। एक लखपति जो दस-बीस लाख बना लेना चाहता है, वास्तव में भिखारी है। कोई गाड़ीवान या द्वारपाल जो तीस-चालीस रुपये मासिक पाता है, यदि वह कहे कि यह मेरे लिए काफी है, मेरी जेब सदा भरी रहती है तो वह उस लखपति से कहीं महान् है, उससे धनी है; क्योंकि न उसमें अभाव का देश है, न माँगने की याचक-वृत्ति ।
अतः समृद्धि के वास्तविक सिद्धान्त का रहस्य है अपनी पूर्णता को दृढ़तापूर्वक स्वीकारना, अपने वैभव को स्वीकारना और ईश्वर को पा कर सब-कुछ पा लेने की मनोवृत्ति में, जहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता, नित्य स्थित रहना। एकमात्र यही उपाय है। यही राज है। जिस क्षण से आप दृढ़तापूर्वक इसे स्वीकारने लगेंगे कि आपमें परिवर्तन होने लगा है, आपकी वृत्ति में परिवर्तन होने लग जायेगा।
वृत्तियाँ आपके चिन्तन की ही उपज हैं। आपके जीवन के निर्माण में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आपका चिन्तन ही है, आपके विचार ही हैं। वे भवन का निर्माण करने वाली ईंटों के ढेर के समान स्थूल तथा स्पर्श करने लायक हैं। वे आपके सम्पूर्ण जीवन का निर्माण कर सकती हैं; आपके जीवन में किसी भी तरह की अवस्था पैदा कर सकती हैं। और यदि विचार सही हुए तो वे विचार आपमें स्वस्थ हो जाने की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं।
जैसे व्यक्ति किसी चीज को पकड़ कर उस पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार सम्यक् विचारों में भी कोष-प्रतिकोष के निर्माण की क्षमता है। विक्षत कोष स्वस्थ हो सकते हैं। कोई भी चीज जो आपमें नष्ट हो गयी हो, सम्यक् विचारों से बन सकती है और इसी प्रकार कुविचार आपके अन्तर का जो पूर्ण है, उसे विनष्ट कर रुग्ण बना सकते हैं।
विचार-शक्ति एक ऐसी चीज है जो आपमें से, प्रत्येक जीवात्मा में से स्फुटित होती है। यह आपके अति-निकट है। आत्म-शक्ति समस्त विचार-शक्ति के मूल में और पृष्ठ में रहती है। अपनी वास्तविक स्थिति को दृढ़तापूर्वक स्वीकारने से आप इतर स्थितियों का तथा उन स्थितियों का जो आपके लिए स्वाभाविक नहीं हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं।
इस उद्देश्य हेतु वैभव की दृढ़ स्वीकृति का वास्तविक रहस्य सन्तुष्टि है। कुछ भी होता रहे , पूर्ण सन्तोष का अनुभव करते रहो। यदि एक रुपया भी हो, तो अनुभव कीजिए कि लाखों रुपये हैं । दस रुपये हों, तो अनुभव कीजिए जैसे दस लाख हैं। यदि एक बार भी आपमें सन्तोष-वृत्ति आ गयी, तो तब कोई भी चीज आपको दुःखी नहीं कर सकेगी। लेकिन यदि आपमें सन्तोष-वृत्ति नहीं है, तो आपको फिर कोई भी सुखी नहीं कर सकता।
सम्पन्नता, समृद्धि का वास्तविक रहस्य है अपने वास्तविक अपरिमित स्वरूप को, अपने पूर्णत्व के असली तथ्य को दृढ़ करना। सन्तुष्ट रहिए और मन के सामने लिख कर टाँग दीजिए- "इच्छाओं का प्रवेश निषिद्ध।" "इच्छाओ! बाहर निकल जाओ।" इच्छाओं के उदित होते ही उनकी उपेक्षा कर दोगे, तो देखोगे कि इच्छित वस्तु स्वतः ही आपके पास आती है। इच्छित वस्तु से जिस क्षण मुँह मोड़ लेंगे, वह स्वयं आपका अनुसरण करने लगेगी। यह शाश्वत विधान है। जिन्होंने इस विधान का अन्वेषण कर स्वयं पर प्रयोग किया, उनके जीवन में यह विधान प्रमाणित हुआ है। आप जितनी इच्छाएँ करते जाते हैं, वे उतनी ही बढ़ती जाती हैं। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखिए, हृदयंगम कीजिए।
कोई चीज इससे भी अधिक कुछ ऊँची है। हिन्दुओं का विश्वास है कि विश्व में जो-कुछ है, सब दिव्य है। सब ईश्वर है। "ईशावास्यमिदं...।" आपको लगता होगा कि मैं बार-बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ; परन्तु सत्य तो कभी बदल नहीं सकता। मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि आज मैं कहूँ कि सब ईश्वर हैं और कल कहने लगूँ कि यह सब ईश्वर नहीं है। सत्य नित्य है। यह लाखों बार कहा गया है; क्योंकि न तो उसे कभी सम्यक् रूप से ग्रहण किया जा सका है, न सम्यक् रूप से जिया जा सका है।
"सर्वं खल्विदं ब्रह्म।" प्रत्येक शक्ति ईश्वर है। सांसारिक प्रत्येक घटना ईश्वर है। प्रत्येक प्राणी ईश्वर है। प्रत्येक नाम और रूप ईश्वर है। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह विविध प्रकट रूपों में दिव्य तत्त्व ही है और समृद्धि भी इस विश्व की पालनकर्ती शक्ति का एक साक्षात् रूप है। दैवी शक्ति इस विश्व-प्रक्रिया में प्रथम प्रक्षेपण-शक्ति, रचना-शक्ति के रूप में व्यक्त होती है जो सबको सत्तावान् करती है और तदुपरान्त वह त्रिकाल-भूत, वर्तमान और भविष्य काल-सातत्य में पालक-शक्ति के रूप में क्रियाशील रहती है।
समझे आप, संसार में जो कुछ आता है, उसे यह शक्ति जीवन देती है, उसका पालन करती है और योगक्षेम वहन करती है। वह ईश्वर ही है। और दूसरे छोर पर जब कल्प का अन्त हो जाता है, वही शक्ति जो कुछ यहाँ लाया गया था, सृजित किया गया था, उस सबको विलीन कर लेती है, अव्यक्त की मूल अवस्था में समस्त कल्पित जगत्-प्रपंच को लीन कर देती है।
दिव्य शक्ति का वह केन्द्रीय पक्ष जो संरक्षक है, पालक है, जीवनदाता और योगक्षेम आदि करने वाला है और यह कार्य वह अनेक प्रकार से करता है- हमारे लिए अधिक महत्त्व का है। वह अन्न में है, ऋतु के मेघ और वर्षा में है, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली विपुल राशि में है, उर्वरता में विद्यमान है। हमारे भीतर जठराग्नि में भी मौजूद है जो हमारे भोजन को पचाती और पुष्टि प्रदान करती है। वह सब समुन्नत अवस्थाओं में भी विद्यमान है।
हमें जानना है कि मानव का सम्पूर्ण जीवन अन्ततः ईश्वर द्वारा ही निर्देशित होता है। वह सम्पूर्ण विश्व का अन्तर्यामी है, वही अखिल ब्रह्माण्ड का संचालक है और वही हमारे जीवन का पथ-प्रदर्शक है। समृद्धि के नियम को आदर देने की, नाना रूपों में प्रकट भगवान् को आदर देने की वह आपके जीवन के प्रत्येक क्षण में भिन्न-भिन्न शर्तें लाता रहता है; अतः इन शर्तों को पूरा तो कीजिए।
२५. योग का महत्त्व
साधक के लिए आध्यात्मिक चेतना के विकास में मन प्रधान शत्रु है। मन ही तृष्णा, विक्षेप, अस्थिरता आदि रूपों में सबसे बड़ी बाधा है। यदि मन पूर्णतः स्थिर हो तो उसमें आत्मा की ज्योति पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित होती है। अहंकार कभी भी हमें अपने मूल-स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता। स्मृति की प्रक्रिया भी एक बड़ी बाधा है। मन के इन सभी पक्षों से युक्त अविचार-बुद्धि आत्मा की हनन-कर्ता है। आत्मिक चेतना उसके कारण प्रकट नहीं हो पाती। चित्त (विचार) की एक बड़ी अरोध्य आदत यह है कि वह कार्य में परिणत होना ही चाहिए और हर कार्य मनुष्य के स्वभाव की एक आदत बन जाता है और जब आदतों में निरन्तर फँसे रहे तो वे हमारी अभिन्न अंग हो जाती हैं।
मनुष्य का व्यवहार उसके चरित्र पर निर्भर करता है। प्रत्येक कर्म बाद में प्रतिक्रिया-स्वरूप फलवान् बीज बन जाता है। जीवन यापन करते हुए वह कर्म की एक समूची संरचना निर्मित कर लेता है। वही उसकी नियति बन जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के विचार उसकी नियति को अनुशासित करते हैं तथा चुने हुए विचारों का, सम्यक् चिन्तन का तथा गलत चिन्तन से बचने का कैसा महत्त्व है?
योग-विज्ञान की अन्तिम विधा का लक्ष्य है मन की मूलभूत क्रियाओं के समस्त व्यापार अवरुद्ध कर देना। परन्तु हम तो राग, द्वेष, कल्पनाएँ, ख्याल, विचार-रूपी उसके विभिन्न रूपों के चंगुल में पहले से ही हैं। अतः मूल की ओर बढ़ने से पहले हमें इन शाखा-प्रशाखाओं को काट फेंकना है।
मान लीजिए, आप सिंह से मुठभेड़ करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको जंगल में घूमना पड़ेगा; तब कहीं अन्त में आप उसकी माँद तक पहुँचेंगे। चित्तवृत्ति मन-रूपी सिंह की माँद है। सबसे पहले आपको ईर्ष्या, घृणा आदि उसके जो रूप हैं, उन्हें नष्ट करना है और तब गलत कार्यों के समुच्चय को, जो गलत चिन्तन का ही परिणाम है, सही करना पड़ेगा। यह आक्रमण के दायरे को क्रमशः संकीर्ण करते हुए लक्ष्य तक आ जाने की एक प्रक्रिया है।
अतः मानसिक व्यापार के बहिर्मुखी प्रसार का विच्छेदन करने के लिए पतंजलि ऋषि ने योग का विवेचन किया और बड़े ही वैज्ञानिक विधिवत् तरीके से किया। मनुष्य अपनी स्थूल निम्न आत्मा, जो उसे निम्न स्तर की ओर खींचती है, के साथ एक विचारशील प्राणी है; परन्तु दूसरी ओर उसका मूल अध्यात्म-स्वरूप है। इन दोनों के मध्य में 'बुद्धि-युक्त मनुष्य' है जो मन से चिन्तन करने की क्षमता रखता है। अतः केन्द्र में चिन्तन-शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति है जो अधि-मानव प्रजाति से भिन्न है। अधि-मानव में चिन्तन-शक्ति नहीं होती।
महर्षि पतंजलि ने मनुष्य के मूल-स्वभाव के अध्ययन के परिणाम तो प्रस्तुत किये ही हैं, परन्तु इसके अतिरिक्त-मनुष्य वस्तुतः जिस प्रकार संरचित हुआ है, इसका भी अध्ययन किया और उक्त निष्कर्ष पर आये। उन्होंने मनुष्य का हिन्दू या मुसलमान समझ कर अध्ययन नहीं किया, बल्कि उसे सार्वभौमिक मान कर उसकी उस संरचना का अध्ययन किया है जो उसके पैदा होने से ले कर उसके अस्तित्व के अन्तिम क्षण तक भूतल पर रहेगी। उन्होंने अन्वेषण किया कि मनुष्य का स्वरूप प्रधानतः शुद्ध सत्ता है। वह तत्त्वतः आत्मा है। वह आध्यात्मिक सत्ता है-यह तथ्य चिन्तन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने स्पष्ट हो जाता है।
मनुष्य में आत्यन्तिक सत्य उसकी परम सत्ता है। कोई भी अपनी असत्ता की कल्पना नहीं कर सकता; क्योंकि यदि आप स्वयं के 'असत्' होने की कल्पना करते हैं, तो उस कल्पना को करने वाला भी होना चाहिए। अतः कल्पनाकार वह आत्यन्तिक सत्ता ही है। मनुष्य में आत्यन्तिक अमरणधर्मा तत्त्व वही सत्ता है। 'वह है।' मैं हूँ। मैं केवल सत् हूँ। मनुष्य का यही सारभाग उसके व्यक्तित्व का प्रमुख अंश है। महर्षि पतंजलि को ज्ञात हुआ कि एक प्रमुख अंश कहीं अन्तर में होता है। मनुष्य की प्रथमतः जिस पर दृष्टि जाती है, वह भौतिक सत्ता है।
मानव-प्राणी के सम्बन्ध में हमारी जानकारी उसके आकार-प्रकार के सम्बन्ध की ही होती है। अतः महर्षि पतंजलि ने कहा कि मनुष्य का एक भौतिक स्थूल शरीर होता है। यह मनुष्य का एक पक्ष है। चिन्तनशील मनुष्य उसके भीतर होता है। जीव-सत्ता का मानसिक पक्ष भी होता है जिसे मनोमय कोश कहते हैं। भाव उत्पन्न होते हैं, विचार आते हैं और जीव विचार करने लगता है और उन विचारों को ही अभिव्यंजित करने हेतु शरीर को क्रियाशील होना पड़ता है। मनुष्य का समग्र जीवन इन विचारों की अभिव्यंजना ही है और यह अभिव्यंजना विविध कार्यों के रूप में होती है और इसलिए विचारशील मनुष्य का अस्तित्व है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इनके बीच में सम्बन्ध होता है।
विचारशील मनुष्य और कार्यशील मनुष्य के बीच में कार्य करने की शक्ति होती है। वह बड़ी विलक्षण अदृश्य आन्तरिक ऊर्जा कही जाती है। वही मनुष्य से कार्य करवाती है। मानव-जीवन में व्याप्त यह शक्ति, जिसके अभाव में समस्त इन्द्रियाँ नितान्त निष्क्रिय हो जाती हैं, प्राण-शक्ति कही जाती है। नेत्र प्राण-शक्ति द्वारा ही देखते हैं। कान इसी शक्ति द्वारा सुनते हैं। जिह्वा प्राण-शक्ति द्वारा ही बोलती है।
मृत्यु-काल में जब प्राण प्रत्यावर्तित होते हैं, प्रस्थान की क्रिया आरम्भ हो जाती है। मृत्यु का अर्थ है-शरीर से प्राणों का उड़ जाना। अतः हम लोग वास्तव में बोलते-चालते शव मात्र हैं। प्राण के चले जाने पर हम पूर्ण गतिहीन, अचल हो जायेंगे; क्योंकि शरीर को प्राण ही चालित करता है, वही क्रिया करता है, खाता-पीता है, आमोद-प्रमोद आदि करता है। यह सब प्राण-शक्ति के ही कारण है। मनुष्य का यह तीसरा पहलू है। इसके पृष्ठ में सबका चालक आत्मा है, 'अस्मि' है। परन्तु एक विलक्षण भ्रम पैदा हो गया है। आपने स्वयं को मन से तदात्म कर लिया है। अतः आप स्वयं को मन से अभिन्न, उसका अविभाज्य अंग समझने लगे हैं। यद्यपि कुछ विरले क्षणों में अनजाने ही आप अपने उस साक्षी-स्वरूप का भी अनुभव करते हैं।
जब आप कहते हैं, 'मेरा मन अशान्त है' तब आप अनजाने में ही स्वीकार कर लेते हैं कि एक आप हैं और एक आपका मन है जो अशान्त है। अतः जब आप कहते हैं कि मेरा मन अशान्त है या मैं मन पर नियन्त्रण नहीं कर सकता, तब आप मन से भिन्न होते हैं। ये आपके वास्तविक स्वरूप की सहज अभिव्यक्तियाँ हैं। अतएव भौतिक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश-सत्ता के अस्थायी, क्षणिक और बहिर्वर्ती तथा अवास्तविक पहलू हैं। तात्त्विक पहलू स्वयं 'सत्ता' है। आप स्वयं केवल सत्ता, अजात, नित्य, शाश्वत और पुराण-'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः' हैं। मन के प्रकट होने से बहुत पूर्व भी आप थे। मनोमय कोश, प्राणिक कोश और स्थूल भौतिक (अन्नमय) कोश से आवृत मनुष्य का उसके असली स्वरूप में, विशुद्ध सत्ता-केन्द्र के रूप में अध्ययन करने की प्रक्रिया ही योगाभ्यास कहलाती है। इसलिए अपने स्वरूप को जानने का एकमात्र उपाय योग ही है।
२६. स्वाध्याय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव
धर्मशास्त्रों में उन महर्षियों के उद्गार हैं जो भगवान् के सीधे सम्पर्क में आये और उनसे भौतिक पदार्थों के ज्ञान की अपेक्षा महत्तर ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्रों के रूप में उन्होंने उसी ज्ञान को दिया है। उपनिषद् आदि शास्त्रों में वे सभी अनुभव और भावानुभूतियाँ संकलित हैं जो उन्होंने ध्यान तथा अतीन्द्रिय अवस्था में प्राप्त की थीं। इन ग्रन्थों में उन प्राचीन ऋषियों के अनुभवों का अभिलेखन है जिन्होंने अपने सुनिश्चित प्रयत्न द्वारा स्वयं को अध्यात्म की उच्चतर भूमिका पर प्रतिष्ठित करके सर्वज्ञान के शाश्वत स्रोत को स्पर्श किया था। यही वे ग्रन्थ हैं जो शाश्वत ज्ञान को उद्घाटित करते हैं और जिनका कथन सार्वकालिक है। ये अपरिवर्तनीय हैं। ये ग्रन्थ दिव्य जीवन यापन का ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं जो हमें भौतिक जीवन से ऊपर उठा सकता है। ये हमें सदाचार का रहस्य बताते हैं जो अन्य ग्रन्थों द्वारा कदापि नहीं मिल सकता।
जीवन में दिव्यता को कैसे जगाया जाये और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर कैसे अग्रसर हुआ जाये-यह कानून, चिकित्सा अथवा वाणिज्य आदि के किसी ग्रन्थ द्वारा नहीं सीखा जा सकता। अपनी आत्मा की अमर नियति के निर्माणार्थ आपको विद्यालय आदि अथवा साधारण पुस्तकालयों को भरने वाली पुस्तकों से हट कर अन्य ग्रन्थों की ओर जाना पड़ेगा। आपको आध्यात्मिक ग्रन्थों और उन सन्तों के जीवन की ओर जाना पड़ेगा जिनमें जीवन-सत्य के अमूल्य रत्न निहित हैं। अतः स्वाध्याय शाश्वत ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान-कोष की स्वर्णिम कुंजी है जो हमारे लिए उनका द्वार खोल देती है और साधक को पूर्ण जीवन, अमर जीवन का पथ दिखाती है।
अब स्वाध्याय के मनोवैज्ञानिक महत्त्व और व्यावहारिक मूल्य के विषय में विचार करें। मनुष्य अपने सामान्य जीवन में स्वाध्याय से क्या प्राप्त कर सकता है, इस पर विचार करें। स्वाध्याय का अत्यन्त गम्भीर और बुद्धिसंगत कारण है। हम जानते हैं कि हमारे मन पर प्रत्येक अनुभव की छाप पड़ती है, प्रत्येक अनुभव मन पर अपना चिह्न छोड़ जाता है। ये चिह्न ही बीज बन जाते हैं। आप जानते ही हैं कि वासनाओं के अनुसार मन की वृत्ति किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ऋषियों ने कहा है कि यदि मनुष्य को उन्नति करनी है तथा प्रतिकूल वासनाओं पर विजय पानी है, तो नित्य प्रति मन में आने वाली इन वासनाओं का सामना करने की कोई विधि नियोजित करनी होगी। इन वृत्तियों पर विजय पाने के लिए ही उन्होंने स्वाध्याय करने को कहा है।
स्वाध्याय कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। मान लीजिए, आप किसी लकड़ी के लडे में कील डालें और बाद में आपको मालूम पड़े की वह कील नहीं चाहिए, तब आप उस कील को उखाड़ने की अपेक्षा दूसरी कील ले कर उसे गाड़ने लगते हैं, तब पहली कील निकल आती है और दूसरी कील लट्टे में गड़ जाती है। कुछ-कुछ इसी तरह हर चीज को बाहर निकालने और वासना को निकाल फेंकने में बहुत-सी स्नायविक शक्ति लग जाती है। अतः उसके बदले स्वाध्याय कीजिए।
प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल आप अतीत के भिन्न-भिन्न युगों के महापुरुषों से सम्पर्क स्थापित करने का यत्न करते हैं- ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तियों से जिनके शब्दों में बल होता है; क्योंकि वे शब्द वास्तविक अनुभव से उद्भूत होते हैं। वे रूपान्तरणकारी शब्द होते हैं। अतः जिन महापुरुषों के जीवन्त अनुभव इन शास्त्रों में होते हैं, आप उनके सीधे सम्पर्क में आ जाते हैं। जिन मनीषियों ने ये धर्मग्रन्थ रचे हैं, उनके शब्दों में आध्यात्मिक उद्बोधन की शक्ति रही है। अतः जब आप किसी धार्मिक
ग्रन्थ को पढ़ने लगते हैं, तब आप इस भौतिक जगत् को भूल जाते हैं। अतः स्वाध्याय का अर्थ है धर्मग्रन्थों के प्रणेताओं वाल्मीकि, व्यास आदि के समक्ष बैठना। यह एक प्रकार का सत्संग है। आप जब स्वाध्याय करते हैं, तो ऐसे महापुरुषों में तल्लीन हो जाते हैं जो आत्म-साक्षात्कार की दीप्ति से दीप्त रहे हैं। ये महान् आत्माएँ मर कर अतीत हो गयी हों, ऐसा नहीं है। वे नष्ट नहीं हुईं। वे उस शाश्वत सत्ता से एक हो गयी हैं, अतः उनका व्यक्तित्व शाश्वत है, अमर है। वह नष्ट नहीं हो सकता। उनका वह व्यक्तित्व साधारण मनुष्य के व्यक्तित्व जैसा नहीं होता जिसमें मृत्यु के समय परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार आप अदृश्य रूप में उपस्थित सन्तों के संग सम्पर्क स्थापित करते हैं। प्रबुद्ध सन्तों की रचनाएँ पढ़ने से आपको उनका साहचर्य मिलता है।
उपनिषद् कहता है: "स्वाध्यायान्मा प्रमदः "स्वाध्याय की कदापि उपेक्षा न करो। हमारे ऋषियों ने स्वाध्याय की यह मूल्यवान् प्रक्रिया बतायी है जिससे हम श्रेष्ठतम मनीषियों से सम्पर्क बनाये रखें। स्वाध्याय करते समय यदि आप किसी ग्रन्थ में बड़े तल्लीन हो जायें, तो आपका चित्त पूर्णतः दिव्य सत्ता पर स्थिर हो जायेगा जो स्वयं ही एक प्रकार की सविकल्प समाधि है। उस समय मन से सभी सांसारिक विचार निकल जाते हैं और मन आध्यात्मिक विचारों में डूब जाता है। यदि आप निरन्तर स्वाध्याय करते रहें तो क्या घटित होगा? आप इन विचारों को मन में लायेंगे और इन प्रेरित विचारों से भावनाएँ उत्पन्न होंगी और आपका चित्त भाव-रूपी सम्पदा से भर जायेगा। स्वाध्याय से प्रतिदिन आपमें समुन्नत करने वाले उदात्त भावों का प्रवेश होता है जो विषाद के क्षणों में आपको साहस प्रदान करते हैं। आप विषादग्रस्त हों, तो स्वाध्याय आपमें उत्साह और जोश भरेगा। यह एक प्रकार से भोजन है जो आप अपनी आत्मा के लिए करते हैं।
आप प्रातः से रात्रि पर्यन्त सांसारिक वातावरण में रहते हैं; सांसारिक व्यवहारों में लगे रहते हैं। इसलिए अनेकानेक भावनाएँ पैदा होती हैं और संस्कार बनते हैं। सन्ध्या समय स्वाध्याय कीजिए। उससे अध्यात्म-विरोधी सांसारिक संस्कार निकल जायेंगे। इन्हें बने रहने का अवसर कदापि न दीजिए। अतः स्वाध्याय की एक व्यावहारिक उपयोगिता तो यही है कि अन्तर में आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होते हैं और समस्त सांसारिक भावनाओं पर अधिकार कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय एकाग्रता और ध्यान में बहुत सहायक होता है।
परन्तु किस प्रकार?
मैं आपके समक्ष एक दृष्टान्त रखता हूँ। इस समय हमारा उद्देश्य होता है मन को किसी एक दिव्य विचार पर दृढ़तापूर्वक लगाना। यही भाव प्रार्थना और पूजा में भी होता है कि मन अन्ततः एक विचार में निविष्ट हो जाये। परन्तु मन सदैव नाना अवांछित विषयों को सोचता रहता है।
एक साधारण असंस्कृत मनुष्य का मन अनेक प्रकार की विषय-वासनाओं से भरा रहता है। उसका समस्त चिन्तन इसी संसार को ले कर होता है। वह जानता ही नहीं कि कोई वस्तु इन्द्रियों के अनुभव से बाहर भी सत्ता रखती है या नहीं रखती। मान लीजिए कि आप अनुभव करें कि वास्तविक विकास में, उन्नति में ये विचार सहायक नहीं 55/8 तब आप अच्छे विचारों को लाने और शुद्ध भाव बनाये रखने का प्रयास करते हैं। कभी अच्छे विचार आते हैं तो कभी बुरे। मन मक्षिका की तरह है जो कभी अच्छी वस्तु पर बैठती है, तो कभी थूक पर भी बैठ जाती है। इस तरह आपका मन विभिन्न वस्तुओं के बीच में डोलता रहता है। परन्तु मधुमक्षिका सर्वदा पुष्पों पर ही बैठती है। वह गन्दगी पर कभी नहीं बैठती। मन को भी मक्षिका की प्रथमावस्था से हटा कर तदुपरान्त मधुमक्षिका वाली अवस्था से भी दूर करके उच्चावस्था में प्रतिष्ठित करना है। स्वाध्याय यही करता है। वह मन को केवल उदात्त विचारों से बाँध देता है, उसे बुरे विचारों को प्रश्रय देने का अवसर ही नहीं देता।
मन वही चीज आत्मसात् करता है जो चीज उसके समक्ष बार-बार लायी जाती है। आरम्भ में मन विद्रोह करेगा; परन्तु जब आपको रस मिलने लगता है, तब आप स्वाध्याय के बिना भोजन भी करना पसन्द न करेंगे। स्वाध्याय मानव-जीवन में आवश्यक बन जाता है। यह आपकी वास्तविक सत्ता के लिए आहार है। जब इसकी आदत पड़ जाती है, तब आपकी मानसिक चेतना के क्षेत्र में आध्यात्मिक विचार ही प्रभावशाली रहेंगे। यह स्वाध्याय की गहरी आन्तर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।
२७. अलौकिक घटनाएँ और योग में उनका स्थान
जो गुप्त है, रहस्यमय है, सरलतापूर्वक दिखायी नहीं पड़ता, उसे गुह्य कहा गया है। अदृश्य घटनाओं को ले कर हमें योग के सन्दर्भ में देखना है कि ये कैसे घटती हैं? महापुरुषों ने संसार के जीवन पर उसके बन्धन, उसकी अपूर्णताएँ, अस्थिरता, अशान्ति, पीड़ा, यातना, दुःख तथा अनेकानेक परेशानियों के सन्दर्भ में विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस परिवर्तनशील अवस्था के परे कोई-न-कोई स्थायी अवस्था अवश्य है। सन्तोष और पूर्णता प्राप्त करने की जिस प्रक्रिया का विकास हुआ, उसे 'योग' कहते हैं।
योग आध्यात्मिक सम्पर्क-स्थापना का गहरा प्रयोग है और यह गहरा प्रयोग स्वल्प वर्षों के जीवन-काल में उन समस्त अनुभवों को समेट लेने का है जिन अनुभवों को एक विकासशील व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक लम्बे दीर्घ काल के बाद कर पाता है। इसमें असाधारण दृश्य और अद्भुत घटनाएँ प्रायः घटने लगती हैं। जिस व्यक्ति को समझ नहीं है, उसे पता नहीं चलता कि उसके भीतर क्या घट रहा है, उसे यह सब असाधारण प्रतीत होता है; परन्तु समझदार व्यक्ति को बिलकुल ज्ञात हो जाता है कि इन घटनाओं के घटने का क्या प्रयोजन है? ये घटनाएँ सभी योग-साधकों एवं जिज्ञासुओं के जीवन में नहीं घटर्ती, प्रत्युत उन्हीं के जीवन में घटती हैं जो पूर्णरूपेण अपने रोम-रोम से, हृदय से, मन से, प्राण से योग-जीवन को समर्पित हैं।
विकास-क्रम के बीच में यह प्रकटन, विभिन्न रूपान्तरण एवं परिवर्तन व्यक्ति की सत्ता के पाँचों भिन्न-भिन्न स्तरों पर आते हैं। अनेक परिवर्तन और अनुभव भौतिक स्तर पर होते देखे गये हैं। कुछ परिवर्तन मन और प्राणिक स्तर पर घटित होते हैं, कुछ क्षमताएँ स्वाभाविक क्रम से आ जाती हैं। कुछ घटती हुई घटनाएँ बाहर से दूसरों को भी दिखायी देती हैं, कुछ अन्तर में ही घटती हैं। तीसरे सूक्ष्म स्तर पर, जो मन से भी और गहरे में है, कुछ अन्य घटनाएँ होती हैं। जिन अगणित मानसिक बीज-संस्कारों के साथ आत्मा शरीर त्यागती है तथा अन्य शरीर धारण के लिए प्रयाण करती है, सूक्ष्म शरीर उन बीज-संस्कारों का संचित कोष है। चौथा स्तर आपका आध्यात्मिक स्तर है जहाँ आत्मिक विकास के कारण आपको इस प्रकार के अनेक आभ्यन्तर अनुभव होने लगते हैं। यह स्तर अपेक्षाकृत अधिक आत्मपरक और अन्तर्मुखी होता है, अत यहाँ जो अनुभव होते हैं, उन्हें केवल साधक ही जान सकता है, अन्य लोग नहीं, क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म क्षेत्र है-उसकी सत्ता की गहराइयों में सर्वाधिक गहरा है।
पाँचवाँ स्तर अति-चेतना का है। यह विश्व-चेतना ईश-चेतना है और इस स्तर पर जो घटनाएँ घटती हैं, वे घटनाएँ वास्तविक होती हैं। इस स्तर पर ज्ञानी जन क्रियाशील होते हैं। वे अपने जीवन में जो कुछ भी देखते हैं, वह सब विश्व-चेतना अथवा दिव्य चेतना के इस सर्वोच्च स्तर की महिमा और शक्ति का प्राकट्य ही होता है। और यह अवलोकन भी वे व्यष्टि-रूप में नहीं, प्रत्युत परम सत्ता-रूप में करते हैं। उक्त पाँचों स्तरों पर गुह्य घटनाएँ घटती दिखायी देती हैं।
योग-साधना निष्ठापूर्वक आरम्भ की जाती हैं, तो फिर चाहे वह योगासन जैसी कसरतें और प्राणायाम ही क्यों न हों विविध आश्चर्यजनक परिणाम लाती है। यदि व्यक्ति लगनपूर्वक आसनों का ही अभ्यास करे और इस अभ्यास को तब तक करता जाये, जब तक वह 'आसन - जय' ('आसन-जय' योग का एक विशेष शब्द है, जिसका अर्थ है लगातार तीन घण्टे अचल, स्थिर हो आसन लगाये रखने की क्षमता।) न कर ले, तो आसन-जय के साथ ही वह समय- समय पर असाधारण अनुभूतियों से गुजर सकता है। योग का अर्थ है-शुद्धता में प्रगति करते जाना। विश्व के समस्त पदार्थों का सत्त्व, रजसू और तमस् में यौगिक विभाजन हुआ है। इच्छा-शक्ति और विवेक द्वारा अपनी क्रियाओं और वासनाओं पर नियन्त्रण कर हम समत्व, ज्योति और शुद्धता की चरम अवस्था तक उठ जाते हैं और जिस समय यह प्रक्रिया चालू रहती है, उस समय विभिन्न नाड़ियों द्वारा चैतसिक ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं और इसके घटित होते ही एक नवीन नाड़ी-प्रवाह, जो अभी तक निष्क्रिय था, शरीर में सत्त्व की प्रधानता होने के कारण क्रियाशील हो जाता है। शरीर में उसकी प्रतिक्रिया होती है और बहुधा झटके लगते भी अनुभव होते हैं।
जिन लोगों ने, चाहे थोड़ी ही मात्रा में की हो, परन्तु यथार्थ में साधना की हो, ऐसे लोग चाहे योग का नाम भी न जानते हों और योग का नाम सुने बिना ही साधना के नाम पर केवल शारीरिक व्यायाम ही करते रहे हों, ऐसे व्यक्तियों के लिए मन-प्राणिक स्तर पर यह जान लेना कि उनमें कुछ क्षमताओं का विकास हो गया है, अति-साधारण अनुभव है। इन आन्तरिक क्षमताओं में सबसे साधारण क्षमता दूसरों के मन के विचार जान लेने की है।
आप चाहे किसी से बात कर रहे हों; परन्तु उसके बोलने से पूर्व ही आप जान लेंगे कि वह क्या कहने जा रहा है? आप रिसीवर उठा कर फोन पर कुछ बात करें, तो ठीक वही बात दूसरा व्यक्ति भी चित्त में ला रहा होता है। बातें करते समय आप दूसरों के मन को भाँप लेते हैं। यह अतीन्द्रिय ज्ञान है। टेलीपैथी है। विकसित की हुई टेलीपैथी नहीं, स्वतःजात टेलीपैथी। आप दूसरों की मानसिक गतिविधि से अनजाने में ही सम्पर्क आरम्भ कर देते हैं। सम्पर्क स्थापित करते हुए भी आपको भान नहीं होता कि आप उनके मानसिक क्रियाकलाप से सम्पर्क कर रहे हैं। यह स्वतः जात टेलीपैथी यों ही घट जाती है। यह सबसे आरम्भ की और सबसे साधारण अलौकिक घटना है और यह मानसिक तल पर घटती है।
दूसरा अनुभव 'अतीन्द्रिय दर्शन' (Clairvoyance) है। यह भी साधारण है। अनेक लोग वे वस्तुएँ देख सकते हैं जो अति-दूर होती हैं। 'अतीन्द्रिय श्रवण' (Clairaudience) उसे कहते हैं, जिसमें आप अचानक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं कि आप दो सौ किलोमीटर दूर बैठे आदमियों की भी बातें सुन सकते हैं।
ये क्षमता के निम्न स्तर हैं। जब किसी के प्राण सूक्ष्म और मन विशुद्ध हो जाता है, तब ऐसी घटनाएँ स्वभावतः ही होने लगती हैं। अनेक बार व्यक्ति को उनका पता भी नहीं चलता और यदि पता चलता भी है, तो वह उन्हें असाधारण नहीं समझता, स्वाभाविक ही समझता है। व्यक्ति के अन्दर जब किसी शक्ति या क्षमता का क्रमशः वर्धन होता है, तब वह उसके असाधारण होने के प्रति सजग नहीं होता और उसे स्वाभाविक समझता है। योग की यह सब आरम्भिक शक्तियाँ हैं और अपेक्षाकृत अधिक त्वरित गति से आती हैं।
व्यक्ति में आकर्षण-शक्ति उस समय आती है, जब कुछ और अधिक विकास हो जाता है। और जिस समय उसका मनो-प्राणिक स्तर से सूक्ष्म शरीर की ओर विकास होने लगता है, तब दूसरी शक्तियाँ विकसित होती हैं। रोग-मुक्त करने की शक्ति तथा किसी को तत्काल आकर्षित कर लेने की क्षमता सूक्ष्म शरीर के तल पर आती है। आपकी प्रगति चाहे बहुत धीमी ही क्यों न हो, ये शक्तियाँ, जो आध्यात्मिक स्तर की शक्तियों जैसी बिलकुल नहीं होतीं, विकसित होने लगती हैं।
ये शक्तियाँ (सिद्धियाँ) मानसिक, मन प्राणिक और सूक्ष्म-तीन तलों की होती हैं। इनका सम्बन्ध योग की जीवन-पद्धति से हो ही, यह कुछ आवश्यक नहीं होता। केवल प्रयत्न द्वारा भी ये शक्तियाँ अर्जित की जा सकती हैं। यदि कोई कृत-सकल्प हो इस ओर यथावश्यक प्रयत्न करे, तो इन शक्तियों को विकसित कर सकता है। योग में ये शक्तियाँ शुद्धिकरण के माध्यम से आती हैं या फिर इच्छा-शक्ति द्वारा। कुछ लोग योग के किसी नियम को नहीं मानते, लेकिन वे ये शक्तियाँ रखते हैं। कुछ लोग केवल चमत्कारवादी (Occultist) होते हैं और सम्मोहन तथा जादू आदि को व्यवसाय बनाये रहते हैं। इस प्रकार वे जो शक्तियाँ विकसित करते हैं, उनसे उनके स्वभाव के परिष्कार अथवा आध्यात्मिक पथ पर प्रगति का कोई संकेत नहीं मिलता।
विश्व-मन से हम सबका सम्पर्क है; क्योंकि हम सब उसी के हैं। हमारी चेतना उस विश्व-चेतना का अंग है, परन्तु अहं-भाव में आबद्ध होने के कारण हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। परन्तु जब कभी हम इस अहन्ता से ऊपर उठने का यत्न करते हैं, तब हमारे मन को विश्व-मन से जोड़ने वाला और हमारी चेतना को विश्व-चेतना से युक्त करने वाला माध्यम और अधिक स्पष्ट हो जाता है और हम एकत्व का अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं। जिस समय यह घटता है, उस समय साधारण चित्त के लिए जो ज्ञान परोक्ष रहता आया है, उसे प्राप्त हो जाता है और सुदूर का ही नहीं, प्रत्युत भविष्य का भी बहुत कुछ ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। क्षमता-विकास का एक निश्चित स्तर आ जाने पर आन्तरिक आध्यात्मिक सत्ता के क्रियाशील एवं आध्यात्मिक स्वभाव के जाग्रत हो जाने पर चेतना का जो विस्तार होता है, उस चेतना विस्तार के कारण यह क्षमता आ जाती है।
यह सम्पूर्ण प्रक्षेपित विश्व सूक्ष्म तत्त्वों से उद्भूत हुआ है। वे सूक्ष्म तत्त्व हैं- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश सबसे सूक्ष्म है। इस सूक्ष्मतम सार-तत्त्व से बाद में दृश्य जगत् की रचना वाले स्थूल तत्त्वों का प्रकटीकरण हुआ। इन स्थूल और भौतिक तत्त्वों का स्रोत अदृश्य और नितान्त सूक्ष्म विश्व-सत्ता है। योग के दौरान यदि योगी इनमें से एक से अधिक तत्त्वों पर एकाग्र हो कर ध्यान करता और समाधि में चला जाता है-जब वह संयम नामक तिहरी क्रिया कर सकने योग्य हो जाता है, तो वह इन तत्त्वों पर अधिकार कर लेता है। वह विद्युत्-गति से आकाश में विचरण कर सकता है, अग्नि और जल के प्रकोप का सामना कर सकता है; क्योंकि इन तत्वों के मूल-स्रोत पर उसका पूरा अधिकार हो चुका होता है और इसे आप एक अलौकिक घटना के रूप में देखेंगे जो कतिपय योगियों की अपरिवर्तनीयता के रहस्य को भी स्पष्ट कर देती है। जल और अग्नि के बीच से गुजरते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उनसे अछूते निकल आये। यह तत्त्वों पर संयम करने का ही परिणाम होता है।
जब आपकी साधना कुण्डलिनी योग का रूप ले लेती है और आप हठयोग की आन्तरिक प्रक्रियाएँ आरम्भ कर देते हैं, तब कुण्डलिनी के निम्न चक्रों से उच्चतर गुह्य चक्रों की ओर उठने के कारण साधक में अनेक असाधारण शक्तियाँ आ जाती हैं और उसे अनेक अनुभव होते हैं।
विभिन्न चक्रों में सुप्त जो शक्ति है, वह योग-मार्ग चाहे कर्मयोग का हो, चाहे भक्ति, ज्ञान अथवा राजयोग का, किसी भी मार्ग से साधना करने से तथा शुद्धता के कारण प्रकट हो जाती है। साधना में निष्णात हो जाने पर, योग के अन्तिम बिन्दु पर पहुँच जाने पर आप आठ मुख्य सिद्धियों (शक्तियों) तथा अनेक गौण सिद्धियों यथा अणिमा (स्वयं को अणु के समान कर लेने की क्षमता), महिमा (इच्छानुकूल आकार-वृद्धि की क्षमता), लघिमा (भारहीनता), गरिमा (असाधारण भार-वृद्धि कर लेना) आदि से सम्पन्न हो जाते हैं। उदाहरणार्थ लघिमा के उपलब्ध हो जाने पर यदि मकान की छत से किसी को गिरा दिया जाये तो वह भूमि पर नहीं गिरेगा, प्रत्युत पंख की तरह हवा में तैरता हुआ भूमि तक आयेगा।
ये सभी सिद्धियाँ गौण हैं। योगी इन्हें नहीं खोजता। ये तो प्रलोभन के रूप में आपका नैतिक मूल्य जाँचने आती हैं और आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधक हैं। साधक में ये सिद्धियाँ इतने गुप्त रूप में, छद्म रूप में कार्य करती हैं कि यदि आप आवश्यकता से अधिक जागरूक और आत्म-निरीक्षण करने वाले नहीं हैं, तो आप इनमें ही फँस जायेंगे और दम्भी हो जायेंगे। यह अवगुण आपमें कब प्रविष्ट हो गया, आप जान ही नहीं पायेंगे। इस प्रकार का सूक्ष्म दम्भ और अहं साधक के लिए सबसे बड़ा जोखिम है; क्योंकि यह साधक के लिए महान् घातक शत्रु 'अहं' के मूल तक पहुँचता है और कोई भी चीज जो इस अहं को बढ़ाती है, ईश्वर के सर्वथा प्रतिकूल है। यदि कोई इन सिद्धियों के प्रति सजग नहीं रहता तो ये उसे परमात्मा से विमुख कर देती हैं, उसे पथ-भ्रष्ट करके उसके अहं को बढ़ावा देती हैं।
इस विषय में समस्त योगी-आचार्य, वर्तमान युग में भारत के महान् सन्तों में अग्रगण्य हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी, श्री स्वामी विवेकानन्द, जिन्होंने सन् १८९३ में पश्चिम को भी योग-वेदान्त दिया, उनके गुरु श्री रामकृष्ण तथा अनेकों अन्य सन्त सब एकमत हैं। इनका कहना है कि आध्यात्मिक पथ पर आरम्भ से ही इन मानसिक शक्तियों से सावधान रहो, अलौकिक शक्तियों से सावधान रहो। यदि आप उनके आकर्षण में फँस गये, तो फिर आप गये। आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जायेगा। यदि आप योग को एक बार भी खो देंगे, तो उसे पुनः पाना बड़ा ही कठिन होगा। वे कहते हैं-"अलौकिक (चमत्कारिक) शक्तियों को विष समझ कर त्याग दो।" आध्यात्मिक जीवन में ये शक्तियाँ वस्तुतः विष-तुल्य ही हैं।
उन आचार्यों के लिए तो इस तरह की सिद्धियाँ कुछ महत्त्व रखती रही होंगी जिनके समक्ष साधकों के पथ-प्रदर्शन का और जनता को ईश्वरोन्मुख करके पथ पर लाने का विशिष्ट कार्य था। कभी-कभी ऐसे साधकों के लिए जो मार्ग पर चलने को तत्पर होते हुए भी आस्था की कमी के कारण पीछे हट जाते हैं, गुरु गण इन सिद्धियों का प्रयोग करते रहे हैं और कभी-कभी जन-सामान्य की सहायता भी इनके द्वारा करते रहे हैं; परन्तु जिनके सम्बन्ध में हम बात कर रहे हैं, उन मुमुक्षुओं को ये सिद्धियाँ भ्रष्ट करने वाली होती हैं। असली साधकों के पथ की ये बहुत बड़ी विघ्न हैं। इनमें सत्यता नहीं होती; अतः इनका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है और न ही कोई महत्त्व । अतः मेरा अन्तिम निष्कर्ष यही है कि आप छाया के पीछे न दौड़ें। केवल सार-तत्त्व को पकड़ें। भूसे के पीछे न पड़ कर अन्न को पाने का प्रयत्न करें जो पोषक और जीवनदायक है। केवल भगवान् के लिए जीयें। उसे ही प्रेम करें। उसी परमात्मा, परम सत्ता की खोज में पूरे हृदय से एकाग्र हो कर लग जायें।
आपका हृदय ईश्वर-प्रेम से आप्लावित हो जाये ! सभी महान् गुरु-आचार्यों के आशीर्वाद आपकी विवेक-ज्योति को सदैव बनाये रखें तथा आपके हृदय में सदैव ज्ञान का आलोक रहे! वे सदैव आपके पथ को प्रदर्शित करते रहें, आपको सद्बुद्धि दें, अन्तर का आध्यात्मिक बल दें जिससे आप पथ से भ्रान्त करने वाली इन क्षुद्र सिद्धियों के आकर्षण को जीत सकें!
२८. एकता का आदर्श
हम भारतवर्ष की सन्तान हैं। हम भव्य और उदात्त औपनिषदिक रहस्यमय तत्त्व के उत्तराधिकारी हैं। हमें सुनायी देने वाला यह शंखनाद औपनिषदिक ज्ञान और अनुभव के शिखरों से युगों-युगों से निनादित हो रहा है- 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति', 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।' यह निनाद उनके जीवन्त अनुभव की शक्ति से उद्भूत है और ईश्वर की सत्ता की एकता प्रतिष्ठित करता है। ऋषियों का उन्मुक्त उद्घोष है कि ईश्वर एक है। उन्होंने ईश्वर को इसी रूप में जाना। वे उसे जानते हैं, वे उसे अनुभव करते हैं और एकता के महा-अनुभव में निवास करते हैं। उसी अनुभव में जीते हुए उन्होंने औपनिषदिक ज्ञान और संसिद्धि के शिखरों से उद्घोषणा की : 'एकं सत्'सत्, सत्ता एक है, अद्वैत है।
यह महान् थाती हमारी है। एकता के महा-भाव की पुनः उद्घोषणा करना, इस एकत्व की भाव-तरंगें उत्पन्न करना और आन्तरिक सत्ता की एकता का यह सन्देश विश्व के कोने-कोने में सबके दिलों में ले जाना ही अपने जन्मसिद्ध अधिकार के, अपनी इस थाती के योग्य बनने की सर्वोत्कृष्ट विधि है।
सत्ता एक होने से मानव-जाति भी एक है; क्योंकि विश्व-विधान के अनुसार आन्तरिक रूप से सब एक-समान हैं। बाह्य रूप से, विविधता प्रकृति का विधान है; परन्तु अन्तर में एकत्व अथवा समत्व जीवन का तथ्य है। आइए, इसकी एक सरल परन्तु स्पष्ट विधि से व्याख्या करें। जीवन के समस्त रूपों को लीजिए। बाह्य दृश्य, भौतिक जगत् के समस्त तत्त्वों को ले लीजिए। सृष्ट वस्तुओं की समस्त प्रजातियों को ले लीजिए। आप पायेंगे कि वे पृथ्वी पर सब जगह तत्त्वतः एक हैं। आकाश हर जगह एक ही है, चाहे वह जगह ईसाइयों की हो, बौद्धों की हो अथवा चीन या जापान की हो। विश्व-भर में जल वही है, पृथ्वी वही है, सूर्य का प्रकाश, वायु, वृक्ष-राशि, वन, प्रकाश, अन्धकार, सूर्य, नक्षत्र और चन्द्रमा वही हैं। विश्वभर में प्रकृति की सभी शक्तियों में नितान्त एकता, समानता, सादृश्य और समता है।
जल-जन्तुओं की असंख्य किस्में हैं; परन्तु मछली समान ही है, चाहे प्रशान्त महासागर की हो, हिन्द महासागर की हो अथवा अन्ध महासागर की। मक्खी, मच्छर, चींटी, चिड़िया, भुनगे किसी की भी कल्पना करें, आप पायेंगे कि हर जगह वे तत्त्वतः एक-समान ही हैं। भारत के केले दक्षिण अफ्रीका या अमरीका के केलों से किंचित् भिन्न लगते होंगे, परन्तु प्रजाति उनकी एक ही है। बहिर्गत वैविध्य तो प्रकृति का विधान है। अतः भारत के भिन्न-भिन्न भागों में केले भिन्न-भिन्न तरह के भिन्न-भिन्न ऋतुओं में पाये जा सकते हैं; परन्तु सृष्टि के आरम्भ से ही समस्त विश्व में शताब्दियों पूर्व से प्रजातियाँ चली आ रही हैं और भविष्य में भी बनी रहेंगी। ये सर्वत्र एक-सी ही हैं। इस प्रकार प्रकृति का अध्ययन करने पर आप पायेंगे कि समानता या एकता एक ऐसा तथ्य है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, वह अपरिहार्य विधान है।
यह विधान मनुष्य के सम्बन्ध में भी ठीक बैठता है। मानव जाति एक है। उसकी प्रजातियाँ एक हैं। मानव जाति की एकता एक ऐसा तथ्य है जिससे किसी तरह बचाव नहीं। हमें इसे स्वीकारना है। निरीक्षण हमें बलात् इस निष्कर्ष पर ले ही आता है।
एक ओर तो सम्पूर्ण विश्व में मानव जाति की एकता है और दूसरी ओर ऋषियों के ऐसे कथन हैं: 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' - ईश्वर एक है। इस प्रकार दो छोर एकता में स्थापित हो जाते हैं, इन दोनों के बीच का क्षेत्र, इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के कार्य का और पारस्परिक सम्बन्धों का क्षेत्र और जीवन तथा इसके अनुभवों तथा सम्बन्धों की प्रक्रियाएँ जिन्हें हम धर्म का नाम देते हैं, स्वभावतः एक ही होना चाहिए और उसे उसी विधान से अनुशासित होना चाहिए। विशुद्ध एकता में एकत्व का लक्षण होना चाहिए। अतः जब हम इस निरीक्षण-परीक्षण के उपरान्त इस दृष्टिकोण से धर्म के तथ्यों में जाते हैं, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्मों में प्रतीयमान चाहे कितना ही अन्तर क्यों न हो, धर्म की प्रक्रिया निश्चित रूप से एक-समान रहती है।
अब देखें जो निष्कर्ष हमने निकाला, वह वस्तुतः सही है अथवा नहीं। प्रथमतः इसे परखने की कोशिश करें कि धर्म की प्रक्रिया वस्तुतः एकतापरक है अथवा नहीं। वह एकतापरक है। किसी भी प्रक्रिया के तीन अंग माने जाते हैं; प्रयोजन जिसे लक्ष्य में रख कर कोई क्रिया की जाती है, क्रिया-विधि के पृष्ठ में निहित प्रेरक शक्ति और ध्येय जिसे यह प्रक्रिया उपलब्ध करने का प्रयत्न करती है। धर्म के सम्बन्ध में ये तीन पक्ष अन्ततः कुछ इस प्रकार प्रतीत होते हैं।
धर्म के अस्तित्व के पीछे क्या उद्देश्य है?
यह पार्थिव अस्तित्व के अशान्तिदायक जंजाल से पलायन की इच्छा है। आप सब धर्मों को जाँच लीजिए। उनमें से हर एक धर्म किसी मानव-व्यक्तित्व से, किसी दैवी पैगम्बर से निकला है या फिर प्रागैतिहासिक काल से चला आया एक शाश्वत विधान है। पृथ्वी पर मानव जाति का कोई भी धर्म क्यों न हो, हम देखते हैं कि सबके मूल में जो प्रेरक शक्ति है, वह है इस भौतिक जीवन को सन्तप्त करने वाली यातनाओं से, कष्ट, वेदना, दुःख, निराशा, व्याधि, मृत्यु, विछोह, विषाद आदि जिन्हें हिन्दू-धर्म 'तापत्रय' कहता है, उनसे पूर्ण इस भौतिक जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा। मुख्य ध्येय है मृत्यु के चंगुल से निकल कर दुःख के पार जा, दुःखातीत अवस्था को, सीमातीत, बन्धनातीत अवस्था को उपलब्ध हो जाना। तमाम धर्मों का यही उद्देश्य है।
जो धर्म में विश्वास करता है, धर्म का जीवन यापन करता है, उसे परम धाम का आश्वासन दिया जाता है जहाँ पहुँच कर जीवात्मा दुःख और अभाव से मुक्त हो जाती है। उसे किसी चीज का अभाव नहीं रहता। दुःख का पूर्णतः अन्त हो जाता है और तब न पीड़ा रहती है, न मृत्यु व्यापती है। मृत्यु का भय चला जाता है। प्रत्येक धर्म अपनी तरह से इस चरम परिणति का आश्वासन देता है। मुसलमानों की धारणा के अनुसार हम बहिश्त के से आनन्द को प्राप्त करते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार हमें परम पिता परमेश्वर के सिंहासन के निकट गौरवशाली शाश्वत स्थान प्राप्त होता है जिसे पा कर मनुष्य एकबारगी कष्ट, पीड़ा, दुःख और मृत्यु के पार हो जाता है। बौद्ध परम निर्वाण को, अपार शान्ति को प्राप्त होते हैं। औपनिषदिक मान्यता के अनुसार सच्चिदानन्द का दिव्यानन्द है जहाँ मनुष्य अमर, भय-रहित, ज्योति से पूर्ण, नित्य आनन्द से पूर्ण हो जाता है। हर धर्म अन्ततः परम ध्येय के रूप में असीम शान्ति, अनन्त आनन्द और परम प्रकाश की ओर लक्ष्य करता है।
धर्म की प्रक्रिया मनुष्य को इस पीड़ा और मरणधर्मा पार्थिव सत्ता से बाँधने वाले कारणों से मुक्त करती है। प्रक्रिया इन कारणों से मुक्त करने की है। यदि अधर्म दुःख का कारण है, तो धर्मपरायण हो जाइए। अधर्म को त्याग दीजिए। यदि असत्य के कारण मनुष्य इस त्रासदायक मरणशील जीवन से बँधता है और यातना तथा पीड़ा के रूप में उसे भुगतना पड़ता है, तो असत्य को त्याग दीजिए। सत्यवादी बन जाइए। यदि हिंसक बनने के परिणाम-स्वरूप आपको दुःख, दर्द, यातना मिलती है, तो आप हिंसा त्याग दें और अहिंसा अपना लें।
भले बनिए, दयालु बनिए, सहृदय बनिए। इस विधि से इस भू-जीवन के तथा भू-जीवन के दुःख, वेदना, यातना आदि के मूलभूत कारण तत्त्वों का अध्ययन करके धर्म की प्रक्रिया विकसित होती है। सन्तों का इसी पर जोर है कि धर्म को व्यावहारिक बना लेने से, व्यवहार में ले आने से आप इन कारणभूत तत्त्वों को नष्ट कर सकते हैं। जागरूक हो कर ऐसा जीवन यापन कीजिए कि आपके द्वारा वे कार्य न हो सकें जिनका परिणाम यह कष्टदायक अस्तित्व है। ऐसा करने पर मनुष्य के वे कार्य उसको आसुरी या पाशवी शक्ति के हाथ का खिलौना नहीं बनने देते।
धर्म की प्रक्रिया धीरे-धीरे मनुष्य के लिए जीवन की एक योजना बनाती है और मनुष्य को अपनी पाशवी वृत्तियों पर विजय पाने तथा अपने दिव्य स्वरूप के दिव्य पक्ष के जीवन-रूपान्तरणकारी उन भव्य तत्त्वों की क्रमशः अभिव्यक्ति के लिए बाध्य करती है जो पहले से ही उसकी आन्तर चेतना के साथ जुड़े हैं। मनुष्य ईश्वर की अनुकृति है; अतः भागवत तत्त्व उसके वास्तविक स्वरूप में हैं। इस कारण आसुरी वृत्ति के बाह्य व्यापार को पूर्णतः दूर फेंक देना चाहिए, निराकरण कर देना चाहिए और इस प्रकार अपने दिव्य स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त अवकाश देना चाहिए।
मनुष्य में जिस समय दिव्य चेतना का विकसन और प्रफुल्लन होता है, उस समय तत्काल ही वह सच्चिदानन्द से जुड़ जाता है। इस प्रकार एकत्व भाव जो अज्ञान से; मल, विक्षेप और आवरण से आवृत था, पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है। यह अनुभव की पूर्णता और साधना की पराकाष्ठा से सम्भव हो पाता है। परम साधना ईश्वर के साथ नित एकता की खोज करती है। मुख्य प्रयोजन, साधना-प्रक्रिया और लक्ष्य-ये तीन मूलभूत कारण बिलकुल इसी तरह सभी धर्मों में पाये जायेंगे।
कोई भी धर्म आपको भू-जीवन से बाँध कर नहीं रखना चाहता। सब धर्मों का लक्ष्य पूर्णता, मोक्ष और अमरत्व में पहुँचना है। सब धर्मों की साधना-प्रक्रिया भी तत्त्वतः समान ही होती है, चाहे उनके बहिर्विस्तार में भिन्नता हो। सब धर्म मनुष्य की निम्न प्रवृत्ति, पाशवी प्रवृत्ति को निर्मूल करना तथा दिव्य प्रकृति का विकास कर देना चाहते हैं जिससे अव्यक्त व्यक्त हो जाये, अन्तर्निहित प्रकट हो जाये और मानव, जो ईश्वर की अनुकृति के जैसा बना है, पुन अपनी वास्तविक स्वरूप की असीमता का भागीदार हो सके। इस अन्तिम ध्येय के सम्बन्ध में सभी धर्म एक हैं।
धर्म या तो अमृत ज्ञान से परिपूर्ण उपनिषद् और वेद जैसे शास्त्रों द्वारा अथवा ईश्वरीय प्रेरणा-प्राप्त महापुरुषों के माध्यम से आया है। यदि हम स्रोत के पास जायें-क्योंकि जो कुछ भी वहाँ से प्रवाहित हो रहा है, उसे जाँचने का उत्तम उपाय स्रोत ही है जहाँ से वह प्रवाहित हो रहा है-और विश्व के विभिन्न धर्मों के स्रोत ईसा, मोहम्मद, जोरस्थुर, कृष्ण या बुद्ध को खोज कर उनके जीवन को जाँचें, तो हम पायेंगे कि अपने व्यावहारिक दृष्टान्तों और आदर्श जीवन में जो कुछ उन्होंने अभिव्यक्त किया है, वह वास्तविक धर्म की आत्मा है।
यहाँ पुनः भव्य और उदात्त एकत्व के दर्शन होते हैं; क्योंकि हर भागवत पुरुष ने अत्यन्त उदात्त ढंग से अपने जीवन द्वारा एक सदाचारी जीवन का, शुद्ध जीवन का, अनन्त करुणा और मधुर प्रेम के जीवन का परिचय दिया है। मोहम्मद, ईसा, बुद्ध, जोरस्थुर आदि दिव्य व्यक्तियों और महा-सन्तों का जीवन भी इन गुणों से पूर्ण रहा है। वे तो प्रेम, मंगल, पवित्रता, ज्ञान, निरासक्ति एवं भ्रातृत्व के साक्षात् अवतार रहे हैं। वे इन गुणों के निष्क्रिय धारक नहीं थे, वरन् उनका जीवन तो इन महान् दिव्य गुणों की सक्रिय अभिव्यक्ति था। संसार में लोगों के बीच में विचरण करते हुए उनके प्रत्येक कर्म और प्रत्येक मुखरित शब्द में ये ही गुण अभिव्यंजित होते थे। उन्होंने धर्म को व्यावहारिक रूप में जीना दिखाया और अपने अनुयायियों को भी सिखाया। धार्मिक जीवन के इस प्रदर्शन में वे सब एक तरह के रहे हैं। सभी ने भागवत जीवन जीया। सभी ने प्रेममय जीवन जीया। सभी ने शुचिता को दीप्ति दी और सभी मनसा वासा-कर्मणा करुणा, सेवा और त्याग में लगे रहे।
आइए, भगवान् के महान् सन्देशवाहकों की भविष्यवाणियों पर विचार करें। क्या ऐसा कोई धर्म है जो हमको झूठ बोलना सिखाता हो अथवा असत्याचरण करने को कहता हो? नहीं है। क्या ऐसा कोई धर्म है जो घृणा और क्रोध बढ़ाने को कहता हो? पुनः उत्तर में कहना पड़ेगा-नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं है। तो क्या कोई ऐसा धर्म है जो अशुद्ध और अनैतिक रहने को कहता हो? इसका उत्तर भी नकारात्मक होगा। इसके विपरीत प्रत्येक धर्म सत्य जीवन का आग्रह करता है। शुद्धता के, ईश्वरपरायणता के, त्याग के जीवन का, करुण कोमल जीवन का आग्रह करता है-ऐसे जीवन का आग्रह करता है जो मनसा-वाचा-कर्मणा कल्याणकारी हो, द्वेष-रहित हो। हर धर्म ने अपने अनुयायियों को परम ध्येय तक पहुँचने हेतु जीवन यापन की एक आदर्श विधि दी है और यह विधि एक-सी ही है। वह विधि है दिव्य जीवन सम्पन्न जीवन। प्रत्येक सन्त के जीवन के व्यवहार में इन गुणों को देखा गया है।
अतः हम चाहे जिस कोण से धर्म-तत्त्व का अध्ययन करें, किसी भी कोण से देखें, हमें पता चलेगा कि धर्म-जीवन एक है, सब धर्मनिष्ठाएँ समान हैं और सब पैगम्बरों ने एक-सा नैतिक पूर्णता का, दिव्य करुणा, भलाई और एकता का जीवन जीया है। वे मानव-जाति के भ्रातृत्व और परमात्मा के पितृत्व की एक-सी भावना ही से प्रेरित हुए थे। अतः इस तथ्य की ओर से हम अपने नेत्र कितने ही बन्द क्यों न रखें, सब धर्मों की एकता इन पैगम्बरों द्वारा जिये आदर्श जीवन के माध्यम से, प्रत्येक धर्म में निहित प्रेरक-शक्ति के माध्यम से और धार्मिक उपलब्धि हेतु आयोजित प्रक्रिया की एकता के माध्यम से अप्रतिहत स्वर में, जीवन्त स्वर में उद्घोषित हो रही है।
यही कारण है कि हमें मनुष्य-जाति के समक्ष सदैव इन दीप्तिमान एक करने वाली कड़ियों को रखना पड़ता है जो सभी मत-मतान्तरों को एक करती हैं। भिन्न-भिन्न मत भिन्न-भिन्न पुष्पों की तरह कहे गये हैं जिनसे एक मनोहर स्तबक बना कर सर्वशक्तिमान् परमात्मा के चरणों में अर्पित किया जाता है। सब मतों के मूल में जो एक करने वाली बातें हैं, उन्हें हम सदा याद रखें और समग्र मनुष्य-जाति में इस एकता की सर्वदा उद्घोषणा करें जिससे संघर्ष, शत्रुता, पार्थक्य-भावना जो इन एक करने वाले मूल-तत्त्वों के दृष्टि से ओझल हो जाने से उत्पन्न हो गयी हैं- एकबारगी ही वसुन्धरा के सुन्दर धरातल से दूर कर दी जायें और मानव जाति में सदैव के लिए शान्ति और सद्भावना व्याप्त हो जाये।
गीता में श्री कृष्ण ने कहा है- "विविध जीव मेरे पास विविध तरह से आते हैं। उनकी भावना के अनुरूप ही मैं उन्हें उपलब्ध होता हूँ।" इस महान् सत्य को स्वीकार करते हुए एक छोटा-सा परन्तु रोचक दृष्टान्त विभिन्न धर्मों और मतों की एकता को प्रभावशाली ढंग से हृदयंगम करने हेतु अप्रासंगिक नहीं होगा।
कुछ लोग यात्रा पर थे और भिन्न-भिन्न दिशा की ओर यात्रा कर रहे थे। गुजरात के एक भक्त ने अपने कार्य से अवकाश लिया। वह विश्वनाथ जी की पूजा के लिए बनारस जा रहा था। दूसरा भक्त आसाम से सेवा निवृत्ति के उपरान्त तीर्थयात्रा पर जाना चाहता है और दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके वाराणसीपुरपति के दर्शन करना चाहता था। कलकत्ते का एक भक्त भी काशी में विश्वनाथ की पूजा करना चाहता है। मद्रास के एक व्यक्ति की भी इसी प्रकार यही आकांक्षा है कि वह वाराणसी जा कर विश्वनाथ की पूजा करे। इस तरह भारत के विभिन्न भागों से आये हुए लोग विभिन्न दिशाओं की ओर विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा कर रहे हैं। एक वाराणसी जाना चाहता है, दूसरा बनारस, तीसरा काशी आदि-आदि। लेकिन तथ्य यह है कि उन सबका गन्तव्य एक ही है, चाहे नाम वे भिन्न-भिन्न दे रहे हैं।
हरेक अपने रास्ते से जाता है। चेट्टियार धनी है; अतः वह दक्षिण से वायुयान लेता है। आसाम का महान् भक्त पूरी यात्रा पैदल करता है। कलकत्ते वाला ट्रेन पकड़ता है। गुजराती किसी और ही तरह के वाहन का प्रयोग करता है। ऋषिकेश से भी एक साधु पैदल बनारस जाता है।
बड़ा महत्त्वपूर्ण तथ्य, जिसे मैं चाहता हूँ कि सब कोई भली-भाँति समझ लें, वह यह है। इसमें सन्देह नहीं कि हर व्यक्ति समझ रहा है कि वह भिन्न स्थान को जा रहा है, यात्रा के उनके साधन भी पृथक् पृथक् हैं; परन्तु उनके यात्रा के बाहरी तरीकों में चाहे कितना ही अन्तर क्यों न हो-योजना सबकी विश्वनाथ के दर्शनों की ही बनी है- क्रमशः उस मुख्य ध्येय तक, विश्वनाथ तक पहुँचने की है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से आप दो आवश्यक तथ्य समझ लें। पहला है, वाराणसी के विभिन्न नाम होने के कारण उत्पन्न इस बात की भ्रान्ति कि भिन्न-भिन्न स्थानों को जा रहे हैं। दूसरा, प्रत्यक्षतः वे विपरीत दिशाओं की योजना बना रहे हैं। कोई दक्षिण की ओर चल रहा है, कोई उत्तर की ओर। गुजरात का व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, आसाम का पश्चिम की ओर। सब प्रतिकूल दिशाओं में जा रहे हैं, लेकिन तब भी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार भिन्न-भिन्न मत सर्वथा विरोधी दिशाओं को चलते प्रतीत होते हैं, परन्तु फिर भी अपने अनुयायियों को उसी लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। एक और बात ध्यान देने की है। मद्रास का चेट्टियार काशी के लिए अपनी यात्रा के दौरान हिमालय के निकट आता जाता है, जब कि ऋषिकेश का साधु, यद्यपि वह भी बनारस जा रहा है, हिमालय से क्रमशः दूर होता जाता है। दो नितान्त विरोधी गतियाँ! परन्तु आश्चर्य है कि दोनों एक-समान ही लक्ष्य प्राप्त करते हैं।
यह दृष्टान्त एक लोकविरोधी बात दर्शाता है कि दो प्रक्रियाएँ, जो परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं तथा जिनके परिणाम भी भिन्न प्रतीत होते हैं, अन्तिम परिणाम में कैसे एक ही लक्ष्य को प्राप्त होती हैं। हर एक की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है; यद्यपि हर एक की धारणा रही थी कि उसने दूसरों से कुछ भिन्न कार्य किया है। एक कहेगा, 'मैं उत्तर की ओर चल कर काशी पहुँचा हूँ।' दूसरा कहेगा, 'मैं दक्षिण की ओर चल कर बनारस आया हूँ।'
इसी तरह सम्पूर्ण विश्व का मूल, आधार एवं अन्तिम लक्ष्य ईश्वर ही है। चेतना के विभिन्न तलों से जीवात्माएँ परमात्मा को उपलब्ध होने चलती हैं और सभी अपने उसी परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाती हैं; दिखायी देने वाली उनकी खोज की साधन-प्रक्रियाएँ चाहे कितनी ही विरोधी या जटिल क्यों न प्रतीत होती हों। धर्म के स्वरूप तथा साधनाओं में विरोधी प्रतीत होने वाली शाश्वत भिन्नताएँ एकता के मूल तत्त्व को नकार नहीं सकीं और न नकारने का कोई कारण ही है। अतएव, अच्छा यही होगा कि हम धर्म की उसी धारणा से लगे न रहें जो हमारा यह परिसीमित मन बनाता है-मन जो अभी तक पूर्ण ज्ञान की अवस्था तक नहीं पहुँच पाया है।
हम महाभारत की उद्घोषणा को याद रखें- "श्रुति का मत भिन्न है, स्मृति का भी। पौराणिक सत्य का, आदि सत्य का सार गुहा में छिपा है। आप सीधे उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अतः समय की सिकता पर पद-चिह्न छोड़ते हुए जिस प्रकार और जिस पथ से महान् आत्माएँ गयी हैं, उसी पथ का अनुकरण कीजिए।"
हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है कि श्रद्धापूर्वक उनकी जीवनियों का अध्ययन करना। उन्होंने अपने उदात्त चरित्र द्वारा जो आदर्श हमारे समक्ष उपस्थित किये हैं, उनका मनन कर स्वयं को उन जीवनादर्शों में ढालने का प्रयत्न करें। मानव जाति की एकता, समस्त धर्मों की एकता और समग्र जीवन की एकता के वास्तविक बोध का यह सबसे महत्त्वपूर्ण तरीका है। विश्वजनीनता, विश्वचैतन्यता (महत्तत्त्व) केवल इसी विधि से प्राप्त हो सकता है।
२९. योग : महत्त्व और स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता
सभी कालों में ईश्वर-साक्षात्कार मनुष्य मात्र की विरासत और उसका जन्मसिद्ध अधिकार रहा है। हमारे ऋषि-मुनियों ने अन्वेषण करके बताया है कि मानव-जीवन का अन्तिम लक्ष्य पूर्णता की प्राप्ति अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर-साक्षात्कार है। अपने घोर परिश्रम, प्रयत्न और खोज द्वारा उन्होंने जो यह अन्वेषण किया था, इसे ही बाद में उपलब्धि की वैज्ञानिक विधि के रूप में गठित कर दिया। उन्होंने जो कुछ स्वतःस्फूर्त साहस से जुट कर तथा बार-बार भूल होने पर भी प्रयत्न करते रहने की प्रवृत्ति द्वारा प्राप्त किया तथा निम्न सत्य के आगे बढ़ कर बृहत्तर सत्य तक (हमारे कल्याण हेतु) पहुँच कर उन्होंने उस सबको आत्म-प्रकाशन और उपलब्धि की एक वैज्ञानिक प्रणाली में, पद्धति में, अभ्यासों की एक श्रृंखला में, व्यवस्था में ढाल दिया जो हमें अन्धकार से प्रकाश में, मृत्यु और मरणशीलता से अमर और शाश्वत जीवन में, दुःख और यातना से दिव्यानन्द की अवस्था में, नित्य सन्तोष, निर्भयता और मोक्ष में ले जाती है, जो 'परमानन्द प्राप्ति सर्वदुःखनिवृत्ति' देती है। यह वैज्ञानिक पद्धति जिसका विकास करके उन्होंने आगामी पीढ़ी को सौंपा, उसे हम योग के नाम से जानते हैं।
ये महापुरुष, ये साहसी अन्वेषक, मनुष्य की आध्यात्मिक आन्तर सत्ता की गहराइयों के ये शोधकर्ता, ये महान् आत्माएँ मृत्यु, पीड़ा और यातना के पार जा सके। आत्म-साक्षात्कार और आत्मज्ञान की अवस्था को उपलब्ध हो जाने पर उन्होंने जागरण का बिगुल बजाते हुए घोषणा की-"अरे मरणशील लोगो ! अश्रुओं की इस उपत्यका में, विलीन होते हुए नाम-रूप के इस जगत् में, क्षणिक, परिवर्तनशील और विनाशशील पदार्थों के इस जगत् में न रुदन करो, न भय करो। हमने मनुष्य की पीड़ा और मृत्यु से भय की समस्या का समाधान खोज लिया है। हम दुःख से पार हो गये हैं तथा हमने उस आदित्य के नित्य प्रकाश का अनुभव कर लिया है जिसे अनुभव करके मनुष्य स्वतन्त्र और मुक्त हो जाता है, अजेय हो जाता है तथा आनन्द और शान्ति से पूर्ण हो जाता है। हम तुमको मार्ग दिखायेंगे, मार्ग का पता बतायेंगे। जो हमने उपलब्ध किया, वह तुम भी कर सकते हो।"
इस प्रकार उन्होंने किसी एक राष्ट्र, जाति या किसी एक विशेष श्रेणी के लोगों अथवा विशेष धर्म को सम्बोधित नहीं किया था, प्रत्युत सम्पूर्ण मानव-जाति को किया था। उन्होंने कहा- "अरे मानव। चले आओ, आओ सुनो, हम तुम्हारे परम कल्याण की बात संक्षेप में बता रहे हैं। हमने उस ज्योतिर्मान् को प्रत्यक्ष देखा है जो मृत्यु से परे है, अज्ञान से परे है और जिसे उपलब्ध हो कर व्यक्ति अमर हो जाता है। जो ब्रहा है, परम सत्य है, समस्त धर्मों का परमेश्वर है, जो अल्लाह के नाम से, जिहोवा के नाम से, स्वर्ग में निवास करने वाले सर्वशक्तिमान् परम पिता के नाम से, आहुरमज्दा के नाम से, ओंकार, तत्सत्, अनाम, केवल के नाम से जाना जाता है, हमने उसे प्रत्यक्ष देखा है। तुम भी उसे प्राप्त कर सकते हो। अतः चले आओ।" सिद्ध महापुरुष मनुष्य को इसी तरह कहते रहे हैं।
योग इस महा-आनन्द की दिव्य अवस्था को उपलब्ध होने की व्यावहारिक विधि है। दुःख और यातना से मुक्त होना कौन नहीं चाहेगा? मृत्युहीन अवस्था को पाना कौन नहीं चाहेगा? जहाँ पहुँच कर मृत्यु की उपेक्षा कर दी जाती है और वह केवल मज़ाक का विषय रह जाती है। जीवन की अशान्ति, व्यग्रता, आपाधापी, तनाव और चिन्ताओं से मुक्त हो गम्भीर स्थिरता और शान्ति-पूर्ण शान्ति, ऐसी शान्ति जिसे कोई भी शक्ति हिला न सके तथा वह आनन्द है जो शाश्वत है, अक्षय है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। ऐसी अवस्था कौन उपलब्ध करना नहीं चाहेगा? मनुष्य की क्या यह सार्वभौन खोज नहीं है?
विश्व में कहीं भी चले जाइए और किसी भी व्यक्ति से पूछिए। मनुष्य-मनुष्य में व्यावहारिक स्तर पर चाहे कितना ही अन्तर हो, चाहे वे हर बात में अन्तर रखते हों, परन्तु इस सम्बन्ध में सब एक होंगे। कष्ट, पीड़ा और शोक से सब बचना चाहते हैं। सभी यथासम्भव अखण्ड आनन्द की पूर्णावस्था चाहते हैं-ऐसी अवस्था जिसका अन्त नहीं होता, जो अस्थायी नहीं, बल्कि शाश्वत है। यह मानव की सार्वभौम खोज है। कोई दुःख भोगना, पीड़ा या यातना सहना नहीं चाहता-फिर चाहे वह पूर्व का हो या पश्चिम का, ईसाई हो या मुसलमान, चाहे वह हिन्दू, बौद्ध, यहूदी, पारसी, कैथोलिक या फिर कम्युनिस्ट ही क्यों न हो। प्रत्येक जाति, उपजाति, मत-मतान्तर और धर्म दुःख और यातनाओं से बचने की इस सार्वजनीन सामान्य इच्छा से जुड़े हैं। वे इनसे बच कर सुख चाहते हैं।
मानव और मानव-स्वभाव की इस सार्वजनीन क्षुधा की तृप्ति के लिए ही समाधान प्रस्तुत किया गया है। हाँ, आपके लिए अनुभव है, आपको चेतना का ऐसा स्तर उपलब्ध करने को है जिसे उपलब्ध कर लेने पर सब-कुछ प्राप्त हो जाता है, जिसे प्राप्त करने की आप जन्म से कोशिश कर रहे हैं और जिसे अभी तक इस नाम-रूपात्मक अस्थायी जगत् में पाने में सफल नहीं हो सके। यह कोई कल्पना की बात नहीं है। आकाश-कुसुम नहीं है जो सदा मनुष्य की पहुँच के बाहर हो। यह सम्भाव्य तथ्य है। एक वास्तविक अनुभव है, सत्य और स्थायी शान्ति है, सत्य और स्थायी आनन्द है जो कभी नहीं जाता। यह दुःख, कष्ट और यातना से पूर्ण मुक्त हो जाने की अवस्था है और पूर्ण सन्तोष, पूर्णत्व का भाव, पूर्ण प्राचुर्य का, भूमा का भाव है। वस्तुतः वही आपका वास्तविक स्वरूप है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।
मनुष्य संसार में कुछ पाने के लिए, रोने, कष्ट भोगने और अन्ततः मृत्यु का, काल का ग्रास बन जाने के लिए नहीं भेजा जाता। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है-क्या आप इन्द्रियों के दास की तरह, इच्छाओं के दास की तरह अथवा अपनी तीव्र वासनाओं के दास की तरह सर्वदा पाशबद्ध रहना चाहते हैं अथवा अपनी निम्न-प्रकृति के बन्धन की इस कारा को तोड़ कर इसी जीवन में परम मुक्ति के क्षेत्र में प्रविष्ट होना चाहते हैं? यह पूर्ण अनुभव की अवस्था किसी दूसरे ही लोक में जा कर प्राप्त हो सकेगी अथवा मृत्यु के उपरान्त प्राप्त हो सकेगी, ऐसी बात नहीं; बल्कि इस अनुभव-प्राप्ति के लिए जो भी सच्चे हृदय से प्रयत्न करते हैं, संघर्ष करते हैं, यह अनुभव उन सभी को प्राप्त हो सकता है-यहीं, इसी जीवन में, अभी इसी शरीर में प्राप्त हो सकता है। योग का यही ध्येय है, प्रभु-कृपा, मुक्ति, इसी जीवन में जीवन्मुक्ति-दुःख और कष्ट से पार जा कर शान्ति की उस अवस्था को उपलब्ध हो जाना जो किसी बाहरी वस्तु से प्रभावित नहीं होती।
'समत्वं योग उच्यते' - सफलता मिले असफलता मिले, मान मिले अपमान मिले, सर्दी हो गरमी हो, सुख हो दुःख हो, कोई अन्तर नहीं पड़ता। दिव्यता की सुदृढ़ भूमि पर पहुँच कर हम सर्वदा एक से रहते हैं। उस समय आन्तरिक शान्ति किसी से भी प्रभावित नहीं होती। जीवन के ऊहापोह, द्वन्द्व भी योग में भली-भाँति प्रतिष्ठित योगी को बिना प्रभाव डाले छोड़ कर विदा हो जाते हैं। यदि आप अन्तर की परम शान्ति की अवस्था चाहते हैं, तो आपको इसके लिए जीवन को संचालित करने की विधि जाननी पड़ेगी। आपको इन विषयों में, दैनिक जीवन के ऊहापोह में ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक तथा आन्तरिक अनासक्ति के साथ उतरना होगा। संसार में होते हुए भी संसार से बाहर रहना होगा। प्रपंचों से सन्निविष्ट होते हुए भी स्वयं को उनमें बाँधिए मत, उनमें फँसिए मत-स्वामी की तरह इन्द्रिय-विषयों के इस संसार में उतर जाइए, सेवक की तरह नहीं जो छोटी-से-छोटी, क्षुद्र-से-क्षुद्र वस्तु के प्रलोभन के सामने, बाह्य आकर्षण के सामने, विषय-वस्तुओं के रंग, रूप, स्वाद, ध्वनि आदि के सामने घुटने टेक देता है। सदैव स्वामी रहो और देखो आत्म-सयम के साथ उनसे कैसे व्यवहार किया जाता है?
आपको जानना होगा कि इन्द्रिय-विषयों के बीच में कैसे रहना है और रहते हुए ज्ञान, विवेक एवं कुशलतापूर्वक कर्म करना है, और करना है आन्तर तटस्थता के साथ। 'योगः कर्मसु कौशलम्' -कर्म में कुशलता ही योग है। भ्रामक आसक्तियों के अन्ध-मोह के इस जजाल में जीवन को न फँसने दीजिए। इसे इन्द्रिय-सुख की इच्छाओं, वासनाओं से मतवाला न बनायें, प्रत्युत आप अपनी उच्च प्रकृति की ओर बढ़े और स्वयं को सर्वदा उसी उच्च प्रकृति में ही प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करें। साथ ही जीवन के प्रति कर्तव्यों को भी पूर्णरूपेण पूरा करते चलें। जीवन के कर्तव्य पूरे होने चाहिए। विधाता ने आपको जिस विशेष परिस्थिति में रखा है, उससे सम्बन्धित आपके जो कर्तव्य हैं, उन्हें आप पूरा करें और बाह्य परिवेश, व्यक्ति या वस्तुओं की उपस्थिति में भी अपनी स्वाधीनता और पूर्णता अक्षुण्ण रखें। यही कर्म में कुशलता है। यही योग है-संसार में रहते हुए भी संसार का न होना।
यदि आप ऐसा करना चाहें, इन प्रलोभनीय विषयों के बीच भी इनसे असम्पृक्त रहना चाहें और स्वयं को आन्तर स्थिरता में प्रतिष्ठित करना चाहें, तो आपको मन को अनुशासित और संयमित करना चाहिए।
आसक्ति और अनासक्ति मन की अवस्थाएँ हैं। साधारण सी बातों से, छोटी-सी घटना के परिवर्तन से उत्तेजित हो जाना या दृढ़, स्थिर, शान्त हो जाना मन की अवस्था पर निर्भर है। अतः मन को संयमित करके तथा श्रेणीबद्ध, क्रमिक तकनीक द्वारा विक्षेप-रहित शान्ति की उस अवस्था की प्राप्ति का क्रमशः प्रशिक्षण देने से उसके स्वभाव में धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। मन के स्वभाव में अशान्ति है, उत्तेजना है। वह सदैव सक्रिय रहता है। अशान्ति से वह अनजान है; क्योंकि वही उसका वास्तविक स्वभाव है। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव जलाने का, जल का बहने का और वायु का गतिशील रहने का होता है, उसी प्रकार मन का स्वभाव सदैव अस्थिर और उत्तेजित होने का है।
लेकिन क्यों!
क्योंकि उसमें कुछ भाग रजोगुण का है। स्रष्टा ने उसे इसी तरह का बनाया है। अतः आपको अपने मन के स्वभाव को बदलना पड़ेगा।
अस्थिर मन की तुलना पारे से की जा सकती है। योग के श्रेष्ठतम ग्रन्थों में से एक में, जिसमें मन के संयम के लिए अनेक विधियाँ बतायी गयी है, एक स्थल पर कहा गया है कि मनुष्य के लिए वायु को पकड़ कर उसकी गति को रोक लेना सम्भव है, परन्तु मन को नियन्त्रित करना कठिन है। मन को नियन्त्रित करना वायु को नियन्त्रित करने से भी और अधिक कठिन है। और इतना कहने के उपरान्त महाचार्य शिष्य को बताते हैं- "मन को इस तरह नियन्त्रित करके उसे सहज करो और समत्व की स्थिति में ला कर शाश्वत सत्य की ओर उन्मुख करो और उस सत्य का ध्यान करो। तुम समस्त कष्टों और दुःखों को जीत लोगे।"
शिष्य कहता है- "आप अत्युत्तम विधि बता रहे हैं; परन्तु विचार में यह व्यर्थ ही है; क्योंकि जिस मन को आप इस तरह उसे नियन्त्रित करने को, समाहित करके ध्यानोन्मुख करने को कह रहे हैं, उसे नियन्त्रित करना असम्भव है।" जब शिष्य गुरु के समक्ष इस प्रकार निवेदन करता है, तो गुरु उससे पूर्णतः असहमत नहीं होते। वह कहते हैं- “तुम ठीक कह रहे हो। निस्सन्देह मन को वश में करना बड़ा कठिन है, मैं भी स्वीकार करता हूँ। यह सरल नहीं है, मैं इसे स्वीकारता हूँ; क्योंकि मैं यह तथ्य जानता हूँ। लेकिन फिर भी असम्भव नहीं है। इस अजेय मन को जीतना भी सम्भव है। अति-कठिन है, पर असम्भव नहीं। इसे नियन्त्रित और अनुशासित करने का कि यह तुम्हारे अधीन हो सके और शान्त तथा स्थिर हो सके-इसका एकमात्र उपाय है, प्रयत्न करना न छोड़ो। यही एकमात्र निदान है। यही करते रहो। प्रयत्न करते रहो, करते रहो। प्रयत्न कभी न छोड़ो।
"योग के तथा एक सच्चे साधक के शब्दकोश में 'असम्भव' शब्द नहीं है। बिना नागा किये अपने प्रयत्न में दिनों-दिन दृढ़तापूर्वक लगे रहो। मन को शान्त, विनियन्त्रित और प्रशान्त करने के प्रयत्न में नियमित रूप से श्रमपूर्वक लगे रहने पर आपको सफलता मिलेगी; परन्तु फिर भी सावधान बने रहने के लिए एक शब्द-जिस समय तुम मन को नियन्त्रित करने का लगातार श्रमपूर्वक श्रम कर रहे हो, उस समय तुम ऐसा कार्य न करो जिससे मन और भी चंचल हो जाता हो। ऐसा करने पर तुम अपने प्रयत्न को विफल कर दोगे। जीवन-काल के एक क्षेत्र में तुम्हें मन नियन्त्रित करना है और दूसरी ओर तुम वे सभी कार्य करने का प्रयत्न करते हो जो मन को और अधिक चंचल बना देते हैं। तब आप ज्वाला को बढ़ा रहे हैं। एक ओर उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं और दूसरी ओर से जल डाल कर उसे बुझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तरीका यह नहीं है।
"दक्षिण भारत में एक कहावत प्रचलित है, जिसका अर्थ है कि 'पालने के शिशु, की आप चिकोटी भी लें और रोने भी न दें।' ऐसा तुम्हें अपने लिए नहीं करना चाहिए, जब तुम शान्त मन से एकान्त में बैठने के लिए सांसारिक विचारों को त्याग कर अपनी चेतना को अन्तर्मुखी कर मन के अनुशासन के लिए थोड़ा समय निकालते हो जिसमें भगवान् के ध्यान और नाम-स्मरण की सहायता से, प्रार्थना अथवा इसी प्रकार के अविरल चिन्तन-प्रवाह द्वारा तुम मौन रहने की चेष्टा करते हो, उस समय तुम्हारा बाहरी सामान्य दैनिक जीवन ऐसा हो कि तुम्हारी वांछित आन्तरिक अनुशासन की प्रगति में सहायक हो। मन में कोई भी विरोधी विचार न आने दो।"
मान लीजिए, आप मन को वशीभूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप छक कर पीने वालों में हैं अथवा बातूनी हैं, साथ ही समाचार-पत्र भी पहले स्तम्भ से आखिरी स्तम्भ तक पढ़े बिना आपसे नहीं रहा जाता। आप विक्षेप डालने वाले अगणित विचारों को तथा जिनसे आपका सम्बन्ध नहीं ऐसी चीजों को भी प्रतिदिन अपने मन में दूँसना चाहते हैं। रेडियो का हर प्रोग्राम सुनते हैं। होता इस प्रकार है; आप मन को प्रतिदिन पहिये की तरह गतिशील रखते हैं। इससे संस्कार बढ़ते हैं। द्रुत गति से घूमते हुए इस 'कैलिडोस्कोप' (नाना-रूपेक्ष) पर आप सांसारिक प्रपंच के अनेकानेक संस्कार लेते जाते हैं। मन को अन्तर्मुखी करने की चेष्टा करें। अनावश्यक कार्यों को कम करने का प्रयत्न करें। जिन वस्तुओं के बिना रहा नहीं जा सकता है, उन्हें भी कम करें। इन्द्रियों को विषय-जगत् में बहुत अधिक जाने से रोकें। अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियन्त्रण रखें।
देखने की चेष्टा कीजिए कि कहीं इन्द्रिय-सुख में बहुत अधिक लिप्त हो कर आप अग्नि में ईंधन डालने का काम तो नहीं कर रहे हैं। इससे मन अशान्त होगा, क्योंकि आप जितना ही अधिक विषय-सुख प्राप्त करेंगे, उतनी ही अधिक कामनाएँ पैदा होंगी और उतना ही अधिक आपका मन अशान्त होगा। अतएव मन के लिए एक ओर से इन्द्रिय-निग्रह की आड़ लगा दीजिए और दूसरी ओर से अपना जीवन सादा बना लीजिए। आवश्यकताएँ कम कीजिए, इच्छाएँ सीमित कीजिए और स्वयं को इस संयम में लगा लीजिए। इस श्रमसाध्य संयम को दिन-प्रति-दिन ननु-नच किये बिना नियमित रूप से करते जायें, साथ ही अपना बाहरी जीवन भी संयम, सन्तुलन, सादगी और बहुत अंशों में निःस्वार्थता का बितायें। ये सभी एक कुलीन, सुसंस्कृत मानव के गुण हैं।
संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान क्या है? स्वयं को नियन्त्रित रखने की क्षमता। यह शिक्षा का सार-तत्त्व है अर्थात् इसके द्वारा व्यक्ति आत्मानुशासन और आत्म-नियन्त्रण में रहना सीखता है। यही वास्तविक सभ्यता की नींव है। सभ्य और असभ्य व्यक्ति में क्या भेद है? सभ्य व्यक्ति आत्मानुशासित होता है। वह अपने पर नियन्त्रण रख सकता है। यदि आपके बाह्य जीवन में सन्तुलन है, सादगी है, आत्म-विनियन्त्रण है, तब आपकी साधना उत्तरोत्तर आपके मन का अनुशासन प्रमाणित कर देगी और तब आपके ये गुण आगे बढ़ते हुए विकास करते जायेंगे। एक दिन ऐसा आयेगा जब आप मन पर विजय पाने में समर्थ हो जायेंगे और जिस दिन आप पूर्ण मनोजय कर लेंगे, उस समय आपका मन स्थिर और समाहित हो जायेगा। यह समाहित मन ही परम सत्य पर ध्यान करता है।
जब मन की समस्त चंचल विचार-क्रियाएँ आपके पूर्णतः वश में हो जाती हैं, तब आप योग की उस अवस्था में उतर जाते हैं जिसे 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' कहा गया है। कामनाएँ, अस्थिर विचार, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, राग, द्वेष, घृणा-ये सब मन की वृत्तियाँ हैं। एक बार भी यदि आप मन को अनुशासित तथा नियन्त्रित करने में सफल हो गये, तो आप अपनी निम्न प्रकृति पर अधिकार कर लेंगे तथा इन नकारात्मक वृत्तियों की अभिव्यक्ति पर भी आपका अनुशासन हो जायेगा। कहने का अर्थ है कि मन के अनुशासन से आप चरित्र का विकास कर लेंगे और आगे चल कर मन आप पर शासन नहीं कर सकेगा, आप उस पर शासन करेंगे, उसके निर्देशक बनेंगे। वह आपको धक्का दे कर हटा नहीं सकता।
आपमें ज्ञान और अज्ञान, सांसारिक तथा असांसारिक, शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा पहचानने की विवेक-शक्ति है। जो-कुछ बुरा है, अवांछनीय है, अशुद्ध है, उसे अस्वीकार करके एक कार्य-प्रणाली को चुन कर उससे एकस्वर हो जाइए जो आपको ऊपर ले जा सके। दिन-प्रति-दिन, प्रतिक्षण, आपके घर में, घर के स्वजनों से आपके सम्बन्धों में तथा आपके व्यावसायिक क्षेत्र में दो तरीके आपके समक्ष सदा उपस्थित होते हैं। प्रथम बड़ा आकर्षक और मधुर और दूसरा है जो आपका उत्थान करता है, आपको सद्गुणी बनाता है, आपके जीवन को उच्च स्तर की ओर ले जाता है तथा जो अन्ततः आपको परम कल्याण तक पहुँचायेगा।
विवेकहीन और आत्म-नियन्त्रण की शक्ति से रहित एक सामान्य मनुष्य प्रतिक्षण प्रिय और आकर्षक वस्तुओं की ओर खिंचता है और अपनी ही वासनाओं, कामनाओं तथा इच्छाओं का शिकार बन जाता है। यही अधोगति का मार्ग है, बन्धन और गहन तमस् का मार्ग है। परन्तु जो मन को अनुशासित और उसकी चंचलता को वश में कर लेता है, उसमें विवेक-शक्ति आ जाती है और वह प्रिय एवं आकर्षक मात्र लगने वाले विषयों से सोद्देश्य और संकल्पपूर्वक दूर हट जाता है तथा श्रेयस् की ओर बढ़ता है।
जो प्रेय और आकर्षक है, आवश्यक नहीं कि वह कल्याणकारी भी हो। जो वास्तव में आपके लिए कल्याणकर है, वह आपको कल्याण की ओर ले जाता है-चाहे वह प्रिय न भी हो। वह कठोर भी हो सकता है। परन्तु विवेक आपको बतायेगा कि कठोर भी आपको अन्तत: परम शुभ और परम कल्याण की ओर ले जा सकता है। वह आपका उत्थान करेगा और अन्तत: लक्ष्य तक पहुँचा देगा। यह योग है-मन पर शासन, चारित्रिक विकास, चिन्तन की स्पष्टता, जो केवल प्रिय और आकर्षक है और गहरे बन्धन में बाँधने वाला है, उसका त्याग और निश्चित रूप से उस आचरण का चुनाव और उसकी स्वीकृति जो आपके जीवन को ऊँचे से ऊँचा ले जाये; क्योंकि योग अन्ततः दिव्य पूर्णता की ओर गतिशील प्रक्रिया है।
आपके अन्तर में दिव्य तत्त्व है, वही आपका वास्तविक और सत्य स्वरूप है। आप केवल यह मनोभौतिक रचना मात्र नहीं हैं जिसे संसार 'व्यक्तित्व' मानता है। यह नाम और रूप, यह शरीर, यह विचार और व्यवहार आपका असली स्वरूप नहीं है। शरीर केवल आवास गृह है और मन केवल वह यन्त्र है जिसके द्वारा आप सोचते और स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। बुद्धि भी बाह्य जगत्-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने का, जीवन-ध्येय के सम्बन्ध में चिन्तन करने का, बुद्धिमत्तापूर्वक जीवन यापन करने और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है।
शरीर, मन और बुद्धि-ये तीन साधन हैं जिनसे आपको सम्पन्न किया गया है। इनका उपयोग करने के लिए, समझदारी से इनका उपयोग करने के लिए ही भगवान् ने आपको यह साधन दिये हैं। परन्तु इन तीनों से परे आप एक शाश्वत स्फुलिंग, अमृत आत्मा तथा दिव्य स्वरूप हैं।
योग आपके अन्तर की दिव्यता का, आपके वास्तविक स्वरूप का प्रकाशन है। आप स्वयं में आते हैं। आप आत्मबोध की अवस्था को उपलब्ध होने के लिए जग रहे हैं। आपको बोध हो रहा है-"मैं अमृतात्मा हूँ, मैं आत्मानन्द हूँ, मैं अस्थि-मांस-मय यह शरीर-पिंजर नहीं हूँ, मैं यह अशान्त और मलिन मन नहीं हूँ जो स्वार्थ से, अहंकार से पूर्ण है, वृथा अभिमान से फूला रहता है तथा काम-क्रोध से, भय और चिन्ता से पूर्ण रहता है। मैं यह ससीम बुद्धि नहीं हूँ जो इतना अधिक विभ्रमप्रवण, इतना अधिक सम्भ्रमशील है, परिमित तथा सीमित है।
"मैं अविनाशी तथा अमर तत्त्व हूँ। मैं इस अशान्त तथा अशुद्ध मन से भिन्न हूँ। मैं नित्य शुद्ध, नित्य शान्तात्मा हूँ। इस सीमित बुद्धि-रूपी साधन से, विवेक-क्षमता- रूपी साधन से भिन्न मैं असीम, सब प्रकार से सम्पन्न, सब तरह से पूर्णात्मा हूँ, आध्यात्मिक चेतना का केन्द्र हूँ जिसमें ज्ञान है, शान्ति है और शुद्धता है, अनादि, अनन्त हूँ जिसके सम्बन्ध में श्रीमद्भगवद्गीता कहती है : 'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे' -शरीर में यह अजात, नित्य, शाश्वत, प्राचीन और कालातीत जीव-सत्ता है जो शरीर के संग नष्ट नहीं होती।"
आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। आप अमर आत्मा हैं जिसका ज्ञान आपको विस्मृत हो गया है। क्या आपको इसका ज्ञान है? क्या आप जानते हैं कि आप अजर, अमर आत्मा हैं? अनादि हैं, अनन्त हैं, कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता, जन्म और मृत्यु आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। ये केवल शरीर से ही सम्बन्ध रखते हैं।
'मैं अजन्मा हूँ, मृत्युहीन हूँ, अमर हूँ, अविनाशी और नित्य हूँ" कैसी उदात्त अवस्था है! यदि इस अवस्था का किंचित् बोध भी आपको हो जाये, तो आप कितने भय-रहित हो जायेंगे! कितने चिन्ता और भय से मुक्त हो जायेंगे ! अन्तर में होने वाले सभी परिवर्तनों के आप साक्षी बन जायेंगे। आप विश्व की विभिन्न अवस्थाओं के, दुःख-सुख के, शीत-उष्ण के तटस्थ साक्षी बन जायेंगे। मन के विकारों के असंग साक्षी बन जायेंगे। मन चंचल है या शान्त, आप उससे दूर रहेंगे। यदि मन अचानक कामनाओं से भर उठता है, तो आप तुरन्त उससे अलग हट कर कहेंगे-"न, मैं तो नित्य शुद्ध, निष्कलंक आत्मा हूँ। अरुचि या आसक्ति मन में घटित हो रही है। मेरा उससे सम्बन्ध नहीं है। मैं नित्य, शुद्ध आत्मा हूँ।"
इस प्रकार आप एक नवीन चैतन्य-बोध विकसित करेंगे जहाँ आप अपने मन की परिवर्तित होती हुई अवस्थाओं के तटस्थ भाव से साक्षी हो सकेंगे।
यही सच्चा जीवन है।
३०. योग और ईसाई-धर्म
आपमें से अधिकांश की पृष्ठभूमि अति धार्मिक और पवित्र ईसाइयत की पृष्ठभूमि है; अतः मैं आपके समक्ष 'योग और ईसाई धर्म' पर ही कुछ विस्तार से बोलूँगा। आपमें से कुछ ईसाई हैं; क्योंकि वे ईसाई ही पैदा हुए हैं। कुछ अधूरे ईसाई हैं। जो हर दो माह बाद गिरजे जाते हैं, परन्तु कुछ भी हो आप सबकी पृष्ठभूमि ईसाइयत ही है, फिर चाहे इनमें कुछ रोमन कैथोलिक हों, प्रोटेस्टेण्ट हों, मेथोडिस्ट हों। कुछ आपमें से यहूदी भी होंगे। तो आप किसी भी मत के हों, जब मैं योग और ईसाई धर्म पर बोलूँगा तो वह योग किसी भी मत पर लागू हो सकेगा।
योग और धर्म में परस्पर क्या सम्बन्ध है?
कुछ मान बैठे हैं कि योग हिन्दू-धर्म का है; अतः उनकी ओर से प्रश्न उठता है-"इस हिन्दू वस्तु का हमारे धर्म से क्या सम्बन्ध है?" अन्य धर्म को मानने वाला हर एक व्यक्ति आश्चर्य करेगा। अतः यह जानने की बात है कि योग को धर्म से कैसे जोड़ें? क्या अन्य धर्मों की भाँति योग भी एक धर्म है अथवा योग और अन्य धर्मों में विशेष भिन्नताएँ हैं? यदि इसका स्पष्टीकरण नहीं होता, तो कुछ लोग अपराध-भावना अनुभव करेंगे और कहेंगे-"ओह, मैं तो ईसाई हूँ। मेरा क्या योग की ओर जाना उचित है? अपनी रूचि के इस योग क्षेत्र में प्रवेश करने से क्या मैं विधर्मी नहीं हो जाऊँगा?" कुछ इस तरह की अशान्तिजनक भावना उसमें उदति होती है।
सर्वप्रथम हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि योग हिन्दू-धर्म की पीठिका से उगा है। इसका उद्गम भारत से हुआ है और यह हिन्दू-धर्म का एक अंग है। लेकिन यह हिन्दू नहीं है। यह सार्वभौम विज्ञान है जो हिन्दू-धर्म की भूमि पर उगा है- यह ऐसा विज्ञान है जो धर्म से ऊपर है, धर्म से श्रेष्ठ है।
यह एक सार्वजनीन तकनीक (विधा) है; क्योंकि पतंजलि के योग-दर्शन के अनुसार षड्दर्शनों में गिने जाने वाले इस योग में न किसी प्रकार की रूढ़िवादिता है और न आपकी पूजा हेतु इसमें कोई देवी-देवता बताया गया है। वह यह नहीं कहता कि आप राम की पूजा करें या शिव की करें अथवा कृष्ण का ध्यान करें और न यही कहता है कि आप दुर्गा, काली या हनुमान् के उपासक हो जायें। इन सबके सम्बन्ध में योग को कुछ नहीं कहना है। वह यह नहीं कहता कि आप भगवान् के किसी विशेष नाम का जप करें। वह केवल यही कहता है कि किसी भी दिव्य नाम के जप से मन एकाग्र होता है। वह दिव्य नाम का जप करने को कहता है। आप ईसा की प्रार्थना कर सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, शिव का नाम ले सकते हैं और यदि आप किसी अन्य धर्म के हैं, तो उसके अनुरूप ही कोई नाम ले सकते हैं। आपको दिव्य नाम का जप करना है। कौन-सा नाम लेना है या किसकी उपासना करनी है, इस विषय में वह कोई निर्देश नहीं देता।
योग का ध्येय और ध्यान का विषय तो वह पूर्ण दिव्य सत्ता है जिसे नित्य-मुक्त, सर्व दोष-रहित, मायातीत, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, सर्वशक्तिमान् स्वर्गपिता, अल्लाह, जेहोवा-किसी भी नाम से पुकारें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह नित्य-मुक्त सत्ता है जो माया से आबद्ध नहीं और दुःखातीत है, सच्चिदानन्द है। अतः आपके अपने ध्येय के अतिरिक्त योग आपको कोई दूसरा ध्येय नहीं बताना चाहता, आपके धर्म के लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं बताता।
वह किसी ऐसे ईश्वर की ओर इशारा नहीं करता जो आपको अपने धर्म, ईसाइयत, मुसलिम आदि धर्म में इंगित की हुई सत्ता से भिन्न हो और न ही उस सत्ता को कोई खास नाम ही देता है कि आपको ईश्वर बदलना पड़े। उस ईश्वर को वह कोई विशेष नाम नहीं देता। हिन्दुत्व की धरती से उठ कर योग धर्म का अतिक्रमण कर लेता है।
योग धार्मिक विज्ञान है अर्थात् वह धर्म से आगे जाता है और विश्वव्यापी तत्त्व का रूप ले लेता है। दूसरे, योग पाश्चात्य या पौर्वात्य लोगों के लिए न हो कर, मनुष्य मात्र के लिए है, सारी पृथ्वी के मनुष्यों के लिए है। यह इस जन्म-मरण और कष्टों से पूर्ण पृथ्वी पर मरणधर्मा मनुष्य को दिया गया है। इस पृथ्वी के मनुष्यों को दिया गया है, फिर चाहे वे मनुष्य कैसे भी हों, कोई भी हों। प्रत्येक काल के लिए दिया गया है; यह नहीं कि केवल प्राचीन युग के लिए ही दिया गया हो या मध्य युग के लिए अथवा आधुनिक युग के लिए ही दिया गया हो, प्रत्युत हर व्यक्ति को, जो समस्त दुःखों, कष्टों और यातनाओं से पार जाना चाहते थे, बन्धन और व्यामोह के पार होना चाहते थे- उन सभी को यह योग दिया गया है। यदि व्यक्ति योग-पथ को ग्रहण कर लेता है, तो योग उसे परम अनुभव में संस्थित कर देता है। अतएव, योग इस भूलोक के मानवों की माँग और आवश्यकता की पूर्ति है। यह कुछ वह चीज है जो मानव-जाति की सम्पत्ति और विरासत कही जा सकती है। योग मानव जाति की विरासत है। यह धर्म में अड़चन नहीं डालता।
योग आखिर करता क्या है?
योग मनुष्य को जीवन देता है, जीवन सप्लाई करता है तथा धर्म से गिरते हुए मनुष्य और मनुष्य से गिरते हुए धर्म में जो कमी आ जाती है, उसकी पूर्ति करता है। यह कह नहीं सकते कि धर्म मनुष्य की उच्चतम आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ है या मनुष्य ही धर्म से लाभ उठाने में, धर्म का भली-भाँति उपयोग करने में असमर्थ हैं, परन्तु इससे एक स्थिति अवश्य ही पैदा हो गयी है।
कुछ लोग कहते हैं कि धर्म असफल हो गया है। मैं कहता हूँ, नहीं। मनुष्य धर्म के कारण दुःख नहीं भोगता, प्रत्युत धर्म का तिरस्कार करने से, धर्म की, धर्म के उपदेशों की, उसके ज्ञान की उपेक्षा करने से दु ख भोगता है। स्थिति प्रायः यही है, परन्तु धर्म जहाँ पूर्णतः संस्थागत, सम्प्रदायगत हो गया है, वहाँ वह एक बड़ा ही निर्वैयक्तिक ढाँचा बन कर रह गया है और परिणामतः व्यक्तियों से अपने जीवन्त सम्बन्ध खो बैठा है। उसके अधीन हो वह अपने वास्तविक महत्त्व से रहित हो जाता है और केवल औपचारिक, रूढिप्रधान, कर्मकाण्डी और तथाकथित धार्मिक संस्कारों के क्रियान्वयन का नमूना मात्र रह जाता है।
आप ईसाई हैं और कहते हैं- "मैं ईसा के रक्त के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने में विश्वास करता हूँ।" तो मेरा विश्वास है कि आप ईसाई हैं, बड़े अच्छे ईसाई हैं; अतः उसी मार्ग से चलते जाइए। जो चाहे कीजिए, मद्यपान कीजिए, धूम्रपान कीजिए, चाहे दसों उपदेशों (Ten Commandments) का उल्लंघन कीजिए, फिर भी आप ईसाई हैं। धर्म का अर्थ हो गया है कि उन वस्तुओं को स्वीकार भर कर लेना जिन्हें किसी धार्मिक सम्प्रदाय ने धर्म में केन्द्रीभूत कर दिया है-जैसे रूढ़ि-विशिष्ट मत आदि-आदि। और आप यदि इन सबको स्वीकार कर लेते हैं, तो आप सच्चे धार्मिक हैं। परन्तु तब यह धर्म नहीं होता।
प्रत्येक धर्म में एक आध्यात्मिक तत्त्व होता है जिसका सीधा सम्बन्ध आपकी आन्तर सत्ता से, आपकी अन्तरस्थ सत्ता से, वास्तविक तात्विक सत्य से होता है। यहाँ धर्म जीवन-सत्ता के उस भाग को स्पर्श नहीं कर पाता और उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, तब वह केवल आपकी जीवन यापन की पद्धति से, सामाजिक जीवन की, पारिवारिक जीवन की पद्धति से ही सम्बन्ध रखता है। उसका सम्बन्ध इतना ही है कि आप अपनी आय का दशमांश देते हैं, आप नियमित रूप से प्रति-सप्ताह गिरजा भी जाते हैं और नित्य पूजा-पाठ करते हैं। आपका बपतिस्मा हो गया और आप ईसाई बन जाते हैं। महत्त्व केवल इसे ही दिया जाता है, आपके श्रेष्ठ अंश को नहीं दिया जाता। आपसे वह कभी स्वयं से प्रश्न करने को नहीं कहता कि आप पूछें कि 'मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मुझे क्या उपलब्ध करना है? मेरे जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है?'
संगठित धर्म में धर्म का कलेवर आपको यह प्रश्न पूछने को उत्साहित नहीं करता, न इस प्रश्न को उठाने और इसका उत्तर माँगने का आग्रह करता है जिस उत्तर से जीवन उस महान् लक्ष्य की खोज बन जाता है जो लक्ष्य आप उक्त उत्तर प्राप्त कर सुनिश्चित करते हैं। ऐसी स्थिति में धर्म आपके जीवन की ऊपरी सतह को ही स्पर्श करता है, अन्तर की गहराइयों को प्रभावित नहीं करता। वह आपकी सत्ता के उस आयाम को स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो पाता जो आपकी वास्तविक सत्ता है। दूसरे आयामों को छुआ जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है, परन्तु यह आयाम अस्पर्शित ही रह जाता है।
अतः जब धर्म में आध्यात्मिक तत्त्व सक्रिय नहीं रह जाता, विकासशील नहीं रह जाता, तब धर्म निष्प्राण हो जाता है। उस अवस्था में वह जीवित नहीं रहता। योग इसका बड़ा अद्भुत उत्तर है; क्योंकि योग का मुख्य सम्बन्ध आपकी आध्यात्मिक सत्ता से है, आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति से है जिसके लिए आपने यह मानव-जीवन पाया है। योग का मुख्य लक्ष्य यही है। योग ईश्वर-साक्षात्कार का पथ है। योग दिव्य अनुभव का पथ है और दिव्य अनुभव धर्म का मर्म है।
ब्रह्म-साक्षात्कार का प्रयत्न ही धर्म का मर्म, धर्म का सार-तत्त्व है। धर्म का यह आन्तर आध्यात्मिक केन्द्र-स्थल है। जब उसी को उपेक्षा भाव से त्यागा और विस्मृत कर दिया जाता है तब धर्म, धर्म का ढाँचा मात्र रह जाता है जिसमें कोई निवास नहीं करता। सैकड़ों घर हों, जिनमें महल एक हो और उसमें कोई न रहता हो, वह वीरान जनशून्य हो-इसी तरह धर्म भी आकार-प्रकार में विशाल इमारत जैसा हो जाता है; परन्तु निष्प्राण, निर्जीव! और यदि वास्तव में किसी का धार्मिक जीवन इस प्रकार का बन गया हो तो चाहे वह ईसाई हो, कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेण्ट हो, यहूदी, पारसी या मुसलमान हो-यदि धर्म ऐसा बन जाता है तो योग उस मरणोन्मुख सूखती हुई आन्तरिक आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक पथ-रूपी लता में जो उपेक्षित होने से सूख गयी है, जीवन-जल सिंचित कर उसे जीवन देने आता है। वह जीवन-प्रदायक शक्ति के रूप में आता है और एक बार आपके धर्म के आध्यात्मिक केन्द्र को पुनरुज्जीवित कर देता है, आपके लिए आपके धर्म को पुनः प्राणवान् बना देता है। चाहे ईसाई हो या मुसलमान, वह सबके धर्म को सजीव बना देता है तथा आपके धर्म में प्राण डाल देता है।
बहुतेरे व्यक्तियों का यह सामान्य-सा अनुभव है कि योग को अपनाने के उपरान्त वे वास्तविक रूप में धार्मिक हो गये। जीवन में योग के आ जाने से ईसाई एक सच्चा भक्त ईसाई हो गया और गिरजा जाने लगा, बाइबिल का पाठ करने लगा, तब ईसा के शब्दों में और अधिक रुचि लेने का यत्न करने लगा और ईसाइयत के नाम पर वह जो-कुछ कर रहा था, उसका अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। पहले इन्हीं कार्यों को उसने व्यर्थ, अर्थहीन कह कर उन्हें यन्त्रवत् की संज्ञा दे कर बन्द कर दिया था। उसमें उसके लिए कोई अर्थ नहीं रह गया था, परन्तु इससे पुनः उसमें अर्थ मिल गया और वह उसमें रुचि लेने लगा और उसके उपदेशों को व्यवहार में लाने लगा। बहुत-सी चीजें जो पहले बिलकुल अर्थहीन थीं, अब पुनः अर्थपूर्ण हो जाती हैं और ईसाई एक अच्छा ईसाई बन जाता है।
योग के द्वारा व्यक्ति को अनेक बार अपने धर्म का आन्तरिक अर्थ समझने में सहायता मिलती है। वह साधना करने का हेतु जानने लगता है और तब अपने धर्म में अधिक रुचि लेने लगता है। योग व्यक्ति को वह धर्म प्राप्त कराने में सहायक होता है जो उस व्यक्ति का अपना धर्म है। वह धर्म का आन्तर आध्यात्मिक तत्त्व पाने में सहायता करता है और समस्त धर्मों की धुरी, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसे प्राप्त कराने में सहायक होता है-उस आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कराने में सहायक होता है जिससे रहित हो धर्म नितान्त बाहरी मुखौटा हो रहता है। योग धर्म को पुनः उसके वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देता है, उसे प्राणवान् बनाता है, हरा-भरा करता है और उसे जीवन में उतार देता है। यह जिस प्रकार ईसाई धर्म पर लागू हो सकता है, उसी प्रकार अन्य किसी भी धर्म पर लागू हो सकता है।
परन्तु अन्तर क्या होगा? इसे भी देख लेना उचित होगा। योग मौलिक पाप (Original Sin) के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता। वह मनुष्य को पापी नहीं कहता। वह मनुष्य को मूढ़ कह सकता है, पर उसे पापी नहीं कहता। मनुष्य भगवान् ही है जो बुद्धिहीन मूढ़ की तरह लीला कर रहा है या फिर मनुष्य भगवान् है जो अपने घर का रास्ता भूल कर इधर-उधर भटकता हुआ, ठोकरें खाता हुआ वर्तुलों में दौड़ रहा है। योग उसके रास्ते को स्पष्ट कर देता है, उस पर प्रकाश डालता है और मनुष्य को पुनः उस रास्ते पर लाते हुए कहता है-"अब, आगे बढ़ो। सीधे अपने घर चले जाओ।" अतः योग नहीं चाहता कि आप अपने को पापी समझें। और दूसरी बात यह है कि दुर्भाग्य से ईसाइयत कुछ क्षेत्रों में नरक से बच निकलने में व्यस्त है, नरक से बच निकलने का प्रयत्न कर रही है और भले ही सर्वथा अनधिकारी हो, पर किसी-न-किसी तरह स्वर्ग-द्वार में प्रवेश करना चाहती है। योग कहता है कि यह बहुत बचकानी बात है। आपके पास इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ कुछ है। यह स्वर्ग और नरक का खेल आप क्यों खेलते हैं?
योग नरक को अस्वीकार करता है, योग स्वर्ग को भी अस्वीकार करता है। स्वर्ग के निर्माता, स्वर्ग के स्वामी की ओर जाइए, स्वर्ग की ओर क्यों जाते हैं? स्वर्ग क्यों चाहते हैं? स्वर्ग की इच्छा भी एक क्षुद्र-सी ही वासना है। आप वास्तव में उसे नहीं चाहते। "मैं ईश्वर को चाहता हूँ। मुझे ईश्वरानुभव चाहिए, मैं ईश्वर को, परमात्मा को, स्वर्ग के स्वामी को अनुभव में ले आना चाहता हूँ।" योग ईश्वर से सम्बन्ध रखता है, स्वर्ग या नरक से नहीं। आप कह सकते हैं कि योग और ईसाइयत में इन्हीं बातों का अन्तर है। यही तथ्य हैं जिनसे रूढ़िवादी ईसाइयत के सिद्धान्तों और योग में भेद है।
योग धर्म को उसके बहुत कीमती अंश से, जो दुर्भाग्यवश विद्यमान नहीं है, पुनः समृद्ध करता है। विश्व के अधिकांश मुख्य धर्मों में उन थोड़े से लोगों को छोड़ कर जो जीवन-पर्यन्त आश्रमों में संन्यासी-संन्यासिनें बन कर रहते हुए किसी-न-किसी प्रकार अपना सम्पूर्ण जीवन अध्यात्म-तत्त्व की उपासना में लगाये रहते हैं- ऐसे लोगों को छोड़ कर सामान्य धर्म में आध्यात्मिक तत्त्व की बहुत बड़ी कमी हो गयी है। परन्तु गत पचास वर्षों से योग के सम्प्रभाव से हम क्रमशः कुछ अपूर्व घटित होते हुए देख रहे हैं। ईसाई-जगत् में इस आन्तरिक आध्यात्मिक पक्ष पर, ईश्वर के साथ अपने सम्बन्ध पर बल देते हुए कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। बहुत से दृष्टान्त सामने हैं।
कुछ तो भगवान् के सन्देशवाहकों की तरह कार्य कर रहे हैं। पूर्व-काल में कुछ पेण्टीकोस्टल (ईस्टर के सात सप्ताह पश्चात् मनाया जाने वाला उत्सव) के जैसे आध्यात्मिक भावोन्मेष से भी भरे रहते थे।
ये सब शुभ लक्षण हैं। योग भी यही कर रहा है अर्थात् धर्म को पुनः धार्मिक जीवन प्रदान कर रहा है। वह व्यक्ति को उसके खोये हुए आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक तथ्य प्रदान कर रहा है- यह महानतम कार्य है जो वह कर रहा है। वह आपके धर्म में अड़चन नहीं डालता, न उसका खण्डन करता है। वह किसी भी चीज का किसी तरह खण्डन नहीं करता। वह कहता है कि आप कहीं भी हों, कोई भी हों, ईश्वर-प्राप्ति का प्रयत्न करें, सजीवन यापन करने की चेष्टा करें। अपनी निम्न प्रकृति का परिष्कार करके उसे शुद्ध बना लें। धर्म प्रदीप्त हो जाय। स्वयं में दिव्य गुणों को उत्पन्न करें और भीतर की दिव्यता को जगा कर प्रभु की ओर बढ़ें। योग का प्रमुख सन्देश यही है। और यह किसी भी धर्म और धार्मिक जीवन के साथ सहज रूप में, सामंजस्यपूर्ण रूप से युक्त हो सकता है तथा युक्त हो कर उसे समृद्ध और सप्राण करके आपको वास्तविक लक्ष्य की ओर जो कि समस्त धर्मों का लक्ष्य है-ले जा सकता है।
३१. श्री स्वामी शिवानन्द जी तथा उनका सन्देश
श्री स्वामी शिवानन्द जी प्रेमपूरित हृदय वाले ऐसे महान् आत्मा थे जो जीवन-पर्यन्त लोगों को सुखी बनाते रहे। उनके जीवन का यही उद्देश्य था और इसी कारण वे अखिल विश्व में असंख्य व्यक्तियों के प्रेमभाजन बने। वे बड़े प्रसन्नहृदय व्यक्ति थे। हँसने और हँसाने में उन्हें आनन्द आता था। बड़े विनोदप्रिय प्रफुल्ल व्यक्ति थे। लोगों के दुःख-शोक को भुलवा कर उनमें आनन्द का आलोक भर देते थे। ऐसा वे हर व्यक्ति के लिए करते थे। वे पूर्व और पश्चिम में, इस जाति और उस जाति में अथवा इस धर्म और उस धर्म में अन्तर नहीं देखते थे।
उनमें महान् करुणा, प्रतिभा और सहानुभूति थी। उनका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का था कि वह लोगों को तुरन्त अनुभव करा देता था कि वे स्वामी जी के हैं और स्वामी जी उनके हैं। विश्व में पराया उनके लिए कोई नहीं था। सब उनके अपने थे। अतः उन्होंने सब पर अपने प्रेम की वर्षा की। यह बड़ा विलक्षण था कि जो लोग उनकी भाषा नहीं समझते थे और जिनकी भाषा वे नहीं समझते थे, वे लोग भी स्वामी जी के समक्ष आते ही उनसे अपने को एक अनुभव करने लगते थे। वे बड़े सरल स्वभाव के थे। अनेक मन्त्रियों, विद्वानों, राजनीतिज्ञों और सार्वजनिक नेताओं ने आ कर उन्हें श्रद्धा और आदर की भावना अर्पित की, लेकिन स्वामी जी ने कभी भी स्वयं को बड़ा, महान् या असाधारण नहीं समझा।
व्यवहार में वे बड़े सहज, सरल एवं लगभग बच्चों की तरह थे। लेकिन इस निरीह सरलता और स्वाभाविकता के संग ही उनके हृदय में अति-गहरा ज्ञान भी था। उन्होंने यह स्वभाव वर्षों की एकान्त कठोर तपश्चर्या और प्रार्थना से पाया था। साथ ही यह भी सही है कि इसके बीज उनमें बाल्यकाल से ही थे। विद्यार्थी-काल में वे बड़े दयालु और परोपकारी थे तथा बड़े-बूढ़ों के, यहाँ तक कि अपरिचितों के भी काम आते थे। तत्पश्चात् डाक्टरी में योग्यता प्राप्त कर वे डाक्टर बने, भारत से बाहर की यात्रा की और सुदूर पूर्व में जा कर डाक्टरी करने लगे। लगभग दस वर्ष डाक्टरी सेवा करते हुए वे सिंगापुर और मलेशिया में रहे। डाक्टरी सेवा के इस काल ने उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन कर दिया। उन्होंने निर्धन रोगग्रस्त लोगों की बिना किसी लाभ की आशा के चिकित्सा-सेवा की।
उन दिनों मलेशिया रबड़ की उपज करने वाले अँगरेजों के हाथ में था। उस विशाल रबड़ की खेती में पूर्व के लोगों को नौकर रख कर काम करवाया जाता था। वहाँ टिन की भी खानें थीं जिनमें लोग काम करते थे। उनमें भारतीय मजदूर, चीनी मजदूर तथा मलेशिया के मजदूर काम करते थे। रबड़ की एक ऐसी ही बड़ी खेती के निकट वे रहते और काम करते थे। अतः वे करुणा, दया और सहानुभूति से प्लावित हो गये। उन गरीब श्रमिकों के कष्ट और यातनाओं से वे विचलित हो पड़े। उनका विशाल हृदय उन श्रमिकों के प्रति सहानुभूति और मैत्री-भावना से भर गया और वे सभी के सुहृद् बन गये। कार्य करते हुए उनके लिए दिन और रात में कोई अन्तर नहीं था। उनका द्वार सबके लिए सदा खुला रहता। किसी बीमार आदमी ने जब कभी उन्हें बुलाया, उन्होंने तुरन्त उसे सहायता दी। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि किसी के बहुत अधिक निर्धन होने के कारण वे स्वयं उसके यहाँ जा कर उसकी शुश्रूषा कर देते। बहुधा अपनी जेब से रुपये भी उन्हें दे देते।
उन दिनों के दौरान उनके व्यक्तित्व का इस प्रकार का विकास हुआ। साथ ही रोगियों के सम्पर्क में आ कर उन्होंने मानवीय दुःख, कष्ट, पीड़ा और मृत्यु जैसी चीजों को जाना और इससे उनमें अन्तर्ज्ञान उदित हुआ। उन्हें इस पृथ्वी के जीवन के वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ। उनके लिए यह कोई सुन्दर या मधुर अनुभव नहीं था। उन्होंने देखा कि यह कष्ट और पीड़ा से, रोग और मृत्यु से पूर्ण है। अतः उनमें धार्मिक चेतना का उदय हुआ। उन्हें लगा कि यहाँ जीवन कष्ट-पीड़ित है, मानव-शरीर दुःख और व्याधियों का घर है तथा आत्मा इस मानव-शरीर में आबद्ध पड़ी है। परिणामतः उनका चित्त अध्यात्म-दर्शन की ओर मुड़ गया। उन्होंने सन्तों और तत्त्वदर्शी महात्माओं के जीवन-चरित्रों और उपदेशों का अध्ययन किया तथा दुःख एवं कष्ट से छुटकारा पाने का मार्ग ढूँढ़ने में लग गये।
"क्या कोई रास्ता नहीं कि मनुष्य अपनी इस वर्तमान दशा का अतिक्रमण कर सके? क्या मनुष्य को अनुभव की केवल यही अवस्था उपलब्ध है या मनुष्य की पहुँच के अन्दर कोई अन्य अनुभव की अवस्था भी है? ऐसी अवस्था जिसमें इस अवस्था की अपूर्णताएँ, यहाँ के दुःख, कष्ट आदि न हों; प्रत्युत जो शान्ति, आनन्द और वास्तविक सुख अभी यहाँ प्राप्त नहीं हैं उनसे पूर्ण हो।”
यह इस तरह की जिज्ञासा और खोज उन्हें दर्शन और चिन्तन की ओर ले गयी और उन्होंने इन प्रश्नों पर बहुत चिन्तन-मनन किया। अन्ततः उनमें ज्ञान का उदय हुआ कि ऐसी अवस्था अवश्य है जो कल्याण से, प्रभु कृपा से तथा शान्ति और आनन्द से परिपूर्ण है और यह अवस्था मनुष्य की पहुँच के भीतर ही है। अतः पूर्व-काल में लोगों ने जो उपलब्ध किया था, वह आज भी किया जा सकता है। और उन्होंने इस परम उपलब्धि के लिए स्वयं को समर्पित करने का संकल्प ठान लिया।
एक दिन अचानक उन्होंने अपनी इतनी चलती हुई प्रैक्टिस को, इतनी ख्याति को, सम्पत्ति को, अपनी प्रत्येक वस्तु को तिलांजलि दी और भारत आ गये। वे एकाकी परिव्राजक की तरह आये और मुड़ कर उत्तर दिशा में हिमालय की ओर चल पड़े। हफ्तों और महीनों की यात्रा के उपरान्त गंगा-तट के एक छोटे से गाँव में पहुँचे जो गंगा के निकट ही चारों ओर पर्वतों से घिरा छोटा-सा स्थान था। एक प्रकार से इस स्थल पर आधुनिक सभ्य भारत की अन्तिम सीमा थी। उसके आगे केवल हिमालय के पर्वत और वन-प्रान्त था। यह भारत का सीमान्त उत्तर भाग था। यहाँ हिमालय की श्रेणियों में भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। इसी स्थल को उन्होंने अपनी एकान्त मौन साधना, तपस्या, उपासना तथा आभ्यन्तर ध्यान-साधना का स्थल बनाया। यहाँ वे सन् १९२३-२४ के बीच में गये थे।
यहाँ वे दस वर्ष ध्यान-मग्न रहे। बहुत कम बोलते थे, आत्म-संयम करते थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे और निकटवर्ती लोगों की बड़े स्नेह और सहानुभूति से सेवा करते थे। वह ऐसा स्थान था जहाँ केवल साधु-संन्यासी ही रहते थे। स्वामी जी उनकी भी सेवा करते थे। आस-पास कुछ गाँव भी थे। सीधे, सरल वहाँ के निवासी थे। स्वामी जी उन लोगों को प्रायः डाक्टरी सहायता देते थे। इसके अतिरिक्त उनका शेष समय पूजा, ध्यान और स्वाध्याय में जाता था। कठिन साधना में व्यतीत हुआ जीवन इस अद्भुत व्यक्ति में आध्यात्मिक प्रकाश ले आया। उस दिन से इस महान् उपलब्धि के लिए मानव-जाति को उद्घोधित करना उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया।
अपने इस आनन्द और शान्ति में वे हर एक को भागीदार बनाना चाहते थे। उन्होंने पुकार कर कहा- "मित्रो, मेरे प्यारे बच्चो, एक तरीका है जिससे तुम इस जीवन के दुःखों, कष्टों से पार जा कर इसी जीवन में वास्तविक शान्ति और सुख प्राप्त कर सकते हो। तुम यहाँ केवल इसे ही प्राप्त करने आये हो। तुम्हारे जीवन का मुख्य लक्ष्य केवल यही है और यही असली जीवन है- जीवन जो तुम्हें महा-उपलब्धि तक ले जाता है, जहाँ पहुँच कर दुःख का अन्त हो जाता है और हृदय आनन्द से भर उठता है, जहाँ पहुँच कर मन की सारी चंचलता का अन्त हो जाता है और उसमें शान्ति आ जाती है, जहाँ जा कर फिर अन्धकार शेष नहीं रहता, अन्तर में ज्योति छिटक जाती है, जीवन दुःखप्रद नहीं रहता, प्रत्युत महातिशय सुख का हेतु बन जाता है।"
अगणित लोगों के जीवन में उन्होंने जो सन्देश पहुँचाया है, उसे उन्होंने 'दिव्य जीवन' का नाम दिया था। उन्होंने सरल, सार्वभौमिक नाम दिया। इस पर किसी धर्म-विशेष का लेबिल (नामपत्र) नहीं चिपका था। जो जीवन आपको दिव्य अनुभव की ओर ले गया, जो जीवन इस ज्ञान में जिया गया कि जो तत्त्व इस भौतिक शरीर और अशान्त मन के भीतर है, वह पूर्णरूपेण दिव्य तत्त्व है, शाश्वत दिव्य तत्त्व है, महा-शान्ति और दिव्यानन्द वाला तत्त्व है। आपके भीतर यह दिव्यता छिपी हुई है। यह अमर आत्मा आपके अन्तर में है। यह शाश्वत सत्ता है। यह देदीप्यमान् विशुद्ध चेतना है। वही आनन्द है। वह शान्ति है। आपके अन्तर में ही आनन्द का यह आधार है। इसे छोड़ कर, इसकी उपेक्षा करके हम इस विषय जगत् में इधर-उधर भटक रहे हैं। ऐसी वस्तुओं में सुख पाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं जो अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, जो त्रुटियों से भरी हैं और व्यर्थ हैं। अनित्य, परिवर्तनशील और ससीम वस्तुएँ किस प्रकार सच्चा आनन्द और सन्तोष दे सकती हैं? यह असम्भव है।
मनुष्य सुख वहाँ ढूँढ़ता है जहाँ वह नहीं मिल सकता। तब वह रोता-चिल्लाता अवश्य है; परन्तु जानता नहीं कि उसके दुःख का कारण क्या है? दुःख का कारण उसी के अन्तर में है। व्यक्ति की यह बड़ी भारी भूल है कि वह समझता है कि यह अपूर्ण संसार उसे वास्तविक सुख देगा और ऐसा समझना ही संसार के सब दुःखों की जड़ है। इस बहिर्जगत् की कोई भूल नहीं है। जगत् आपके समक्ष खड़ा हो कर कहता नहीं कि आओ, मैं तुम्हें सुख प्रदान करूँगा। संसार के विविध पदार्थ भी यह घोषणा नहीं करते कि हम ही सुख के स्रोत हैं और हम ही तुम्हें सुख दे सकते हैं। वे किसी चीज का वचन नहीं देते; अतः वे किसी तरह की निराशा उत्पन्न नहीं करते। आप ही हैं जो उनसे आशा करते हैं और तब निराशा को जन्म देते हैं। अतः त्रुटि जगत् में नहीं, मनुष्य में है। और इस प्रकार मनुष्य जन्म से मृत्यु तक भू-जीवन के अरण्य में, नश्वर और परिवर्तनशील विषयों के मरुस्थल में इस कल्पना के साथ भटकता फिरता है कि इन विषयों में वह यहाँ असली सुख पा लेगा।
ये विषय केवल अस्थायी ऐन्द्रिक सुख दे सकते हैं। एक स्वच्छ, सुन्दर आकृति या वर्ण नेत्रों को किंचित् सुख दे सकता है। कुछ मधुर ध्वनियाँ अथवा प्रिय शब्द कानों को थोड़ा सन्तोष दे देते हैं। मिष्टान्न का स्वाद जिह्वा को किंचित् तृप्ति दे देता है। कुछ सुखद कोमल स्पर्श त्वचा को हलका-सा आनन्द दे जाते हैं। अर्थात् ये किंचित् प्रिय लगने वाले रसास्वाद, सुगन्ध, स्पर्श, श्रवण और दर्शन अल्प मात्र ही इन्द्रिय-सन्तोष देते हैं। यह ऐन्द्रिक सन्तोष सुख नहीं है, आनन्द नहीं है। यह केवल भौतिक स्तर तक ही है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो पूर्णरूपेण आपकी स्नायविक रचना पर निर्भर करती है। स्नायविक रचना इस पशु-ढाँचे का ही एक हिस्सा है।
भौतिक शरीर आपके व्यक्तित्व का पशु ढाँचा ही है। यदि आपकी स्नायु-तन्त्री का कोई भाग काम न करता हो, तो आपको यह संवेदनात्मक अनुभूति नहीं होगी। अतः ये पंचेन्द्रिय अनुभव भौतिक स्नायविक प्रक्रिया के कारण ही होते हैं। इसे सुख नहीं कहा जाता। सुख सत्ता की अन्तर्मुखी अवस्था है; मन और हृदय की आभ्यन्तर्मुखी अवस्था है। कभी-कभी जब कोई कारण भी उपस्थित नहीं रहता, तब भी यह आपके अन्तर से उमड़ता रहता है। कभी-कभी जब आप अकेले बैठे रहते हैं और आपके मन को कोई इच्छा परेशान नहीं कर रही होती, कोई चाहना अन्तर में नहीं होती-आप अपने में शान्त बैठे रहते हैं, ऐसे इन क्षणों में आप अपने अन्तर में एक दुर्लभ उल्लास का अनुभव करेंगे। यह आनन्द विषयों की अनुपस्थिति में आता है।
यह महान् सत्य है कि आनन्द भीतर है और सुख आपकी सत्ता के ही केन्द्र में है जिसे भीतर ही खोजना होगा-बाहर नहीं। व्यक्ति जितना ही बाहर दौड़ता है, आवश्यकताएँ उतनी ही बढ़ती हैं और सुख-शान्ति से व्यक्ति उतना ही दूर हो जाता है। हमारे गुरुदेव के उपदेशों में यह सत्य हर एक को दिया गया है। परन्तु वे एक यथार्थवादी और व्यावहारिक पुरुष थे। अतः यद्यपि उन्होंने आत्म-साक्षात्कार का यह महान् आदर्श प्रस्तुत किया, तथापि वे जानते थे कि मनुष्य को अपना सामान्य जीवन भी यापन करना है। इसलिए उन्होंने दैनिक जीवन यापन हेतु कुछ व्यावहारिक सिद्धान्त भी बताये हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने सामान्य जीवन के कार्यों को, कर्तव्यों को, घरेलू, सामाजिक और व्यवसायगत कर्तव्यों को सम्पन्न करते हुए भी क्रमशः आत्म-नियन्त्रण और आत्मिक अनुशासन की अवस्था में आ जाता है।
यह क्रमिक अनुशासन जो उन्होंने मनुष्य को दिया, इसमें उनके दिव्य जीवन के उपदेशों का सार है। उनके नियम तथा उपनियम साम्प्रदायिक भावना से रहित हैं, अतः वे जिस धर्म में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है अथवा जिस धर्म और निष्ठा की वह साधना कर रहा है, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं डालते। ये दिव्य जीवन के सिद्धान्त ऐसे हैं जो किसी के मत या धर्म को प्रभावित नहीं करते और व्यक्ति उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतार सकता है, आत्मसात् कर सकता है। इन उपदेशों को उन्होंने बीस निर्देशों में एकत्र कर दिया है और इन बीस आध्यात्मिक निर्देशों में उन्होंने सभी सन्त-महात्माओं के उपदेशों का सार-तत्त्व संकलित कर दिया है। उन्होंने बताया कि दैनिक जीवन का यही धर्म है। उन्होंने कहा कि यही धर्म की साधना और धर्म का विज्ञान है और इन नियमों को अपनाने से व्यक्ति सुख-शान्ति की ओर बढ़ता तथा दुःख और कष्टों से दूर हो जाता है।
आप दयालु बनें और मैत्री-भावना से पूर्ण रहें। किसी से घृणा न करें। कोई आपको अप्रिय न लगे। दूसरों में सद्गुण देखिए; उनके अवगुणों पर ध्यान न दीजिए। कोई पूर्ण निर्दोष नहीं है। कोई जिम्मेवार भी नहीं है; क्योंकि वह जैसा भी है, ईश्वर का बनाया है। अतः हर चीज को उदार दृष्टि से देखिए। शुभ देखिए और मिथ्यात्व की उपेक्षा कीजिए। मिथ्यात्व देखना ही हो तो जो स्वयं में है, उसे देखिए। उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए और निर्दोष बन जाइए। इस प्रकार दैनिक जीवन में सहृदयता का अभ्यास कीजिए।
आपकी वाणी क्रोध-रहित और मृदु हो। मधुरता और विनम्रतापूर्वक बोलिए। लोगों को क्षमा कीजिए। सदैव सेवा करने का यत्न कीजिए। सत्यनिष्ठ बनिए और इस प्रकार सबकी निःस्वार्थ सेवा द्वारा, कृपालुता और दयालुता के अभ्यास द्वारा, मधुर वचनों द्वारा अपना हृदय शुद्ध कीजिए। इस अखिल विश्व का जो स्रोत है, उस परम सार्वभौम सत्ता के लिए गहरा प्रेम बढ़ाइए। वही आपकी सत्ता और इस विश्व के अस्तित्व का आधार है। उसके दर्शन करके, उसे उपलब्ध करके व्यक्ति पूर्णता को उपलब्ध होता है। इस वर्तमान स्थिति में, आप अपनी सत्ता के उस स्रोत से विच्छिन्न हो जाने के कारण अपूर्ण हैं। आपके जीवन में पूर्णता और अखण्डता तब आयेगी, जब आप पुनः उससे अपना आध्यात्मिक सम्पर्क और सम्बन्ध बना लेंगे। अतः उसके अनुभव को प्राप्त करने के लिए महा-आकांक्षा और तीव्र लालसा उत्पन्न कीजिए। यह आन्तरिक क्षुधा, यह आन्तरिक भक्ति आन्तरिक जीवन की साधना द्वारा विकसित कीजिए।
अपने अन्तर में सजीव रहिए और आन्तर जीवन का विकास कीजिए। प्रार्थना के माध्यम से, दैनिक चिन्तन के माध्यम से, आन्तरिक भक्ति-भावना द्वारा प्रगति कीजिए और उस परम दिव्य सत्ता को सदैव अनवरत रूप से स्मरण रखने का अभ्यास कीजिए। अपने दैनिक जीवन में भी कीजिए। अपने अन्तर को इसी शाश्वत परम तत्त्व में विश्राम लेने दीजिए। ऐसा जीवन ही दिव्य जीवन कहा जाता है; क्योंकि यह ऐसा जीवन है जो आपको दिव्य अनुभव की ओर ले जाता है। यह जीवन, आपमें जो आपका दिव्य स्वरूप है, उसे प्रकाशित करता है। यह ऐसा जीवन है जो आपके जीवन का जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, उस लक्ष्य-बोध के साथ यापन किया जाता है। यह वह जीवन है जिसमें मन, वचन और कर्म द्वारा आप अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यंजित करते हैं-जीवन जिसमें अन्तर से सौन्दर्य, प्रेम और आनन्द अभिव्यक्त होता है।
अब जीवन आपके क्षुद्र, स्वार्थी स्वभाव की अभिव्यंजना की प्रक्रिया मात्र नहीं रह जाता। वह क्षुद्र कोटि के स्वार्थपूर्ण कार्यों की, क्रोध की झुंझलाहट की, कठोर शब्दों की, लड़ाई-झगड़ों की मनमुटीवल या ईर्ष्या-द्वेष, उग्रता और अशान्ति की प्रक्रिया नहीं रह जाता; बल्कि दयालुता, सहृदयता, मैत्री, प्रेम, निःस्वार्थ सेवापरायणता, दूसरों को सुखी बना देने की इच्छा और दूसरों के लिए अधिकाधिक मात्रा में स्वयं उपादेय बना लेने का जीवन हो जाता है। ऐसा जीवन ही दिव्य जीवन कहा जाता है। आप स्वयं के लिए ही शुभ बन जाते हैं, अपने घर में आनन्द ले आते हैं, अपने माता-पिता और स्वजनों के लिए सुख का साधन बन जाते हैं। अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्रों में, समाज में, अर्थात् अपने कर्म के समस्त क्षेत्रों में आप मैत्री, प्रेम और आनन्द ले आते हैं। आप कल्याण-केन्द्र की भाँति विचरण करते हैं, स्वयं को आनन्द और शान्ति से पूर्ण करते हैं, दूसरों के लिए भी सुख-शान्ति लाते हैं। परन्तु यह सब करने के लिए आत्मानुशासन की अपेक्षा है।
आप अपनी ही इन्द्रियों के दास हैं तो आप ऐसा जीवन नहीं बिता सकते। अतः आपको अपनी इन्द्रियों पर, मन पर, मन की इच्छाओं पर, अहं पर और अहंपरता पर नियन्त्रण करना होगा। लेकिन आप यह न सोचें कि यह नियन्त्रण कुछ संन्यासियों और संन्यासिनियों की कठोर तपश्चर्या जैसा होगा। इससे सर्वथा भिन्न, यह अनुशासन तो वास्तविक सभ्यता का लक्षण है, वास्तविक शिक्षा का सूचक है। स्वयं पर अपना ही इस प्रकार का नियन्त्रण तथा अनुशासन और दूसरों को सुखी करने की महत्त्वाकांक्षा के समक्ष अपनी इच्छाओं का त्याग ही वास्तविक संस्कृति का सार-तत्त्व है। सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति-ऐसे विवेकसम्मत आत्मानुशासन पर ही प्रतिष्ठित हैं। इस तरह का आत्मानुशासन ही जीवन को जीने योग्य बनाता है।
जिस समाज या समुदाय में इस प्रकार के आत्मानुशासित स्त्री-पुरुष रहते हैं, वह समाज या समुदाय वास्तव में समृद्ध और सम्पन्न होता है। यह संसार का निषेध करने वाला दर्शन नहीं है; क्योंकि भूलिए मत, याद रखिए, अस्थायी निषेध से आप सुख और आनन्द की स्थायी अवस्था की ओर बढ़ेंगे। यह संयम और निषेध केवल संयम और निषेध के लिए ही नहीं है; बल्कि जैसा आप जानते हैं, वास्तविक आनन्द की उपलब्धि का यही मार्ग है।
इस प्रकार ध्येय आनन्द है, सुख है, शान्ति तथा परिपूर्णत्व है। यही आत्म-पथ है, यही दिव्य जीवन है।
बीस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नियम
परम श्रद्धेय श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज
१. ब्राह्ममुहूर्त-जागरण - नित्यप्रति प्रातः चार बजे उठिए। यह ब्राह्ममुहूर्त ईश्वर के ध्यान के लिए बहुत अनुकूल है।
२. आसन-पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन पर जप तथा ध्यान के लिए आधे घण्टे के लिए पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। ध्यान के समय को शनैः-शनैः तीन घण्टे तक बढ़ाइए । ब्रह्मचर्य तथा स्वास्थ्य के लिए शीर्षासन अथवा सर्वांगासन कीजिए। हलके शारीरिक व्यायाम (जैसे टहलना आदि) नियमित रूप से कीजिए। बीस बार प्राणायाम कीजिए।
३. जप-अपनी रुचि या प्रकृति के अनुसार किसी भी मन्त्र (जैसे 'ॐ', 'ॐ नमो नारायणाय', 'ॐ नमः शिवाय', 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय', 'ॐ श्री शरवणभवाय नमः', 'सीताराम', 'श्री राम', 'हरि ॐ' या गायत्री) का १०८ से २१,६०० बार प्रतिदिन जप कीजिए (मालाओं की संख्या १ और २०० के बीच) ।
४. आहार-संयम-शुद्ध सात्त्विक आहार लीजिए। मिर्च, इमली, लहसुन, प्याज, खट्टे पदार्थ, तेल, सरसों तथा हींग का त्याग कीजिए। मिताहार कीजिए। आवश्यकता से अधिक खा कर पेट पर बोझ न डालिए। वर्ष में एक या दो बार एक पखवाड़े के लिए उस वस्तु का परित्याग कीजिए जिसे मन सबसे अधिक पसन्द करता है। सादा भोजन कीजिए । दूध तथा फल एकाग्रता में सहायक होते हैं। भोजन को जीवन-निर्वाह के लिए औषधि के समान लीजिए। भोग के लिए भोजन करना पाप है। एक माह के लिए नमक तथा चीनी का परित्याग कीजिए। बिना चटनी तथा अचार के केवल चावल, रोटी तथा दाल पर ही निर्वाह करने की क्षमता आपमें होनी चाहिए। दाल के लिए और अधिक नमक तथा चाय, काफी और दूध के लिए और अधिक चीनी न माँगिए ।
५. ध्यान-कक्ष-ध्यान-कक्ष अलग होना चाहिए। उसे तालेकुंजी से बन्द रखिए।
६. दान–प्रतिमाह अथवा प्रतिदिन यथाशक्ति नियमित रूप से दान दीजिए अथवा एक रुपये में दस पैसे के हिसाब से दान दीजिए।
७. स्वाध्याय-गीता, रामायण, भागवत, विष्णुसहस्रनाम, आदित्यहृदय, उपनिषद्, योगवासिष्ठ, बाइबिल, जेन्दअवस्ता, कुरान आदि का आधा घण्टे तक नित्य स्वाध्याय कीजिए तथा शुद्ध विचार रखिए।
८. ब्रह्मचर्य-बहुत ही सावधानीपूर्वक वीर्य की रक्षा कीजिए। वीर्य विभूति है। वीर्य ही सम्पूर्ण शक्ति है। वीर्य ही सम्पत्ति है। वीर्य जीवन, विचार तथा बुद्धि का सार है।
९. स्तोत्र-पाठ-प्रार्थना के कुछ श्लोकों अथवा स्तोत्रों को याद कर लीजिए। जप अथवा ध्यान आरम्भ करने से पहले उनका पाठ कीजिए। इससे मन शीघ्र ही समुन्नत हो जायेगा।
१०. सत्संग-निरन्तर सत्संग कीजिए। कुसंगति, धूम्रपान, मांस, शराब आदि का पूर्णतः त्याग कीजिए। बुरी आदतों में न फँसिए ।
११. व्रत-एकादशी को उपवास कीजिए या केवल दूध तथा फल पर निर्वाह कीजिए।
१२. जप-माला-जप-माला को अपने गले में पहनिए अथवा जेब में रखिए। रात्रि में इसे तकिये के नीचे रखिए।
१३. मौन-व्रत - नित्यप्रति कुछ घण्टों के लिए मौन-व्रत कीजिए।
१४. वाणी-संयम-प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलिए । थोड़ा बोलिए । मधुर बोलिए।
१५. अपरिग्रह-अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए। यदि आपके पास चार कमीजें हैं, तो इनकी संख्या तीन या दो कर दीजिए। सुखी तथा सन्तुष्ट जीवन बिताइए। अनावश्यक चिन्ताएँ त्यागिए। सादा जीवन व्यतीत कीजिए तथा उच्च विचार रखिए।
१६. हिंसा-परिहार-कभी भी किसी को चोट न पहुँचाइए (अहिंसा परमो धर्मः) । क्रोध को प्रेम, क्षमा तथा दया से नियन्त्रित कीजिए।
१७. आत्म-निर्भरता-सेवकों पर निर्भर न रहिए। आत्म-निर्भरता सर्वोत्तम गुण है।
१८. आध्यात्मिक डायरी-सोने से पहले दिन-भर की अपनी गलतियों पर विचार कीजिए। आत्म-विश्लेषण कीजिए। दैनिक आध्यात्मिक डायरी तथा आत्म-सुधार रजिस्टर रखिए। भूतकाल की गलतियों का चिन्तन न कीजिए।
१९. कर्तव्य-पालन-याद रखिए, मृत्यु हर क्षण आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अपने कर्तव्यों का पालन करने में न चूकिए। सदाचारी बनिए।
२०. ईश-चिन्तन-प्रातः उठते ही तथा सोने से पहले ईश्वर का चिन्तन कीजिए। ईश्वर को पूर्ण आत्मार्पण कीजिए ।
ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः!
यह समस्त आध्यात्मिक साधनों का सार है।
इससे आप मोक्ष प्राप्त करेंगे ।
इन नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए ।
अपने मन को ढील न दीजिए ।