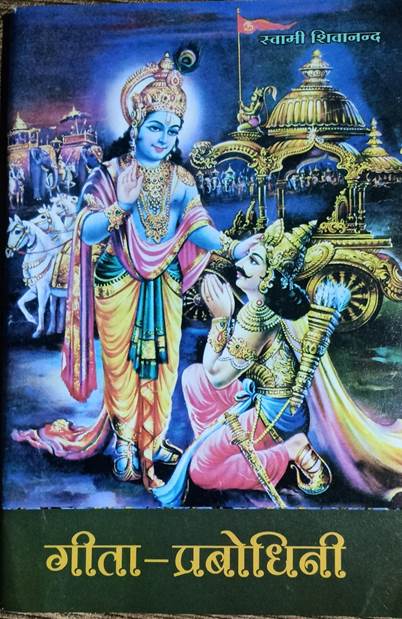
गीता-प्रबोधिनी
THE BHAGAVADGITA EXPLAINED
का अविकल अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती
अनुवादक
श्री रामकुमार भारतीय
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर-249 192
जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण :१९८३
द्वितीय हिन्दी संस्करण : २०११
तृतीय हिन्दी संस्करण : २०१४
(१,००० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
HS 18
PRICE: 55/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए
स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त
फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, शिवानन्दनगर, जि. टिहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड, पिन २४९ १९२' में मुद्रित।
For online orders and Catalogue visit: dlsbooks.org
प्रकाशकीय
श्रीमद्भगवद्गीता के सिद्धान्तों का सम्पूर्ण दृष्टिकोण इस पुस्तक में संघनित रूप में है। भगवद्गीता के सिद्धान्त सम्पूर्ण मानवता के लिए आध्यात्मिक विकास एवं साक्षात्कार हेतु हर युग के लिए सामान्य निर्देशन हैं; किन्तु वर्तमान समय, जब कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति तनावग्रस्त एवं चिन्ता से प्रताड़ित है, इस ग्रन्थ का एक विशेष महत्त्व एवं मूल्य है। भगवद्गीता ससीम आत्मा की पुकारों का उस असीम द्वारा दिया गया उत्तर है। यह केवल धरती के मानव की परिस्थितियों के हल ही प्रतिबिम्बित नहीं करती, प्रत्युत् समस्त वैश्वीय अवस्थाओं का भी हल इसमें सन्निहित है। भगवद्गीता किसी एक धर्म-विशेष की पाठ्य-पुस्तक नहीं, प्रत्युत् धर्म के वास्तविक स्वरूप का ग्रन्थ है। यह उस उच्चतर चेतना की वाणी है जो अपने परिपूर्ण स्वरूप को-परमात्म-स्वरूप को उद्घाटित करती है। प्रस्तुत रचना में द डिवाइन लाइफ सोसायटी के उपाध्यक्ष श्री स्वामी योगस्वरूपानन्द जी महाराज का परिश्रम एवं प्रयास सम्मिलित है।
-द डिवाइन लाइफ सोसायटी
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
गीता-ध्यान
हे जननी भगवद्गीते! मैं आपका ध्यान करता हूँ; क्योंकि महाभारत के युद्ध-क्षेत्र में स्वयं भगवान् ने अपने मुखारविन्द से अर्जुन को आपका आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था। मैं परम ज्ञान-स्वरूप महर्षि व्यास का भी ध्यान करता हूँ जिन्होंने महान् ग्रन्थ महाभारत की रचना की जो 'पंचम वेद' कहलाता है; क्योंकि इसमें मानव का समस्त ज्ञान समाहित है। हे महर्षे! मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ब्रह्माण्ड-चेतना के साथ एकात्म होने के कारण आप भगवद्-उपदेशों को आत्मसात् कर सके। महाभारत हृदय-प्रदीप के तैल के सदृश है। आपने इस दीप को गीता-ज्ञान से प्रज्वलित किया है और इस भाँति लोगों की अपनी दैनिक समस्याओं तथा अज्ञानान्धकार को पराभूत करने में सहायता की है। हे महर्षे! आपको मेरा नमस्कार! आपने महान् ग्रन्थ महाभारत, जो कि व्यष्टि-सत्ता को विश्व-सत्ता के साथ अपने को युक्त करने की विधि की शिक्षा देने के कारण 'योग-शास्त्र' भी कहलाता है, में विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने वाले विभिन्न पात्रों के माध्यम से मानव-मन के विभिन्न प्रकार्यों का बड़ा ही सुरुचिपूर्ण प्रतिपादन किया है। आपने महाभारत युद्ध में पाण्डव-पक्ष की उच्चतर मन से और कौरव-पक्ष की निम्नतर मन से तुलना की है।
महाभारत युद्ध की दुस्तीर्ण सरिता के भीष्म तथा द्रोण दो प्रबल तट हैं। ये दोनों अपराजेय योद्धा थे जिनसे अर्जुन को अत्यधिक अनुराग था जिसके कारण वह विषण्ण और युद्ध में अपना कर्तव्य करने को अनिच्छुक था। हे महर्षे ! आपने तद्वत् शिक्षा दी कि आध्यात्मिक पथ में राग बहुत बड़ा अवरोध है। राजा जयद्रथ ने अनुचित साधनों से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या की तथा युद्ध में भीषण क्रोध का केन्द्र-बिन्दु बना। अतः महाभारत-युद्ध-सरिता के जल की तुलना इस दुष्ट राजा से की गयी है। दुर्योधन तथा उसके भ्राताओं के मामा शकुनि, जिसने द्यूत-क्रीड़ा में कपट से विजय प्राप्तं की थी, की तुलना सरिता-तल पर स्थित एक बड़े नीलोत्पल से की गयी है जो नेत्रों को लुभाता और इस प्रकार व्यक्ति को सरिता के सम्भाव्य संकटों के प्रति असावधान बनाता है। शल्य इस जल में बलशाली ग्राह के सदृश्य है जो दुराक्रम्य है। कृपाचार्य इस सरिता की प्रबल धारा है; क्योंकि उनका शौर्य सेना को वेगवती धारा की भाँति निरन्तर आगे बढ़ने को उत्तेजित करता था। कर्ण, जिसे धनुर्विद्या में अपनी निपुणता के कारण अभिमान था, की तुलना सरिता की उत्ताल तरंगों से की गयी है मानो वे अभिमान तथा दुराग्रह से क्षुब्ध हो रही हों। अश्वत्थामा तथा विकर्ण ने अवैध रूप से पाण्डवों की सेना के अनेक लोगों का संहार किया; अतः वे सरिता में अपने शिकार को निगल जाने वाले मकर हैं। जैसे सरिता में जलावर्त समस्त जल-प्रवाह को अपनी गति की ओर निर्दिष्ट करता है वैसे ही दुर्योधन ने सम्पत्ति, सत्ता तथा पद के लोभ में आ कर पाण्डवों को नष्ट करने के लिए अनेक विश्वासघाती उपायों का प्रयोग किया। इससे आपने यह शिक्षा दी कि सम्पत्ति, सत्ता तथा पद की कामना व्यक्ति के जीवन का पूर्णतया सत्यानाश कर डालती है। आपने विश्व को यह प्रकट कर दिया कि एकमात्र भगवान् तथा उनकी महिमा के सतत स्मरण तथा जैसा पाण्डवों ने भगवान् श्रीकृष्ण को आत्म-समर्पण किया था, उसी भाँति सर्वशक्तिमान् प्रभु को आत्म-समर्पण करने से ही मनुष्य अपने जीवन के दैनन्दिन संघर्षों को पराभूत तथा इस जन्म-मृत्यु के चक्र-रूपी संसार सागर का सन्तरण कर सकता है। जैसे पाण्डव अपने कर्णधार-रूप श्रीकृष्ण की सहायता से महाभारत-रूपी सरिता पार कर गये वैसे ही मुझे शुद्ध मन तथा बुद्धि प्रदान करें तथा अज्ञानान्धकार को पार कर अमरत्व का प्रकाश उपलब्ध करने के लिए भगवान् को सतत स्मरण करने तथा उन्हें आत्म-समर्पण करने को मुझे समर्थ बनायें!
हे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र तथा वृन्दावन की गोपियों को परमानन्द प्रदान करने वाले भगवान् कृष्ण! आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जैसे स्वर्गिक पारिजात वृक्ष की छाया के नीचे जाने से लोगों की मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, उसी भाँति आपने पाण्डव तथा अन्य जिन लोगों ने आपके चरण कमलों की शरण ली, उनके सभी क्लेश विदूरित कर उन्हें निष्काम तथा अमर बना दिया।
हे परम प्रभु! आपने पार्थसारथि के रूप में दोनों सेनाओं के मध्य में अपने एक हाथ में कशा तथा दूसरे हाथ में ज्ञान-मुद्रा धारण कर अर्जुन को भागवत-धर्म का उपदेश दिया। इस ज्ञान-मुद्रा में मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका उँगलियाँ सीधी तथा परस्पर सन्निकट रखी जाती हैं जो प्रकृति के त्रिविध-सत्त्व, रज तथा तम-गुणों की द्योतक हैं। तर्जनी उँगली जीव की द्योतक है। यह अँगूठे की ओर अभिनत होती है और उसे स्पर्श करती है। अँगूठा परम ब्रह्म का प्रतीक है। जब जीवात्मा तीनों गुणों से पृथक् हो जाता है, तब वह ब्रह्म से योग प्राप्त कर लेता है।
हे जगद्गुरो, दुष्टों का संहार तथा साधुओं का परित्राण करने वाले हे भगवान् कृष्ण ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे माधव, हे परमानन्द के स्रोत ! मैं आपको दण्डवत् प्रणाम करता हूँ। एकमात्र आप ही वाक्शक्तिहीन मूक को वाचाल (वाक्शक्ति विशिष्ट) तया गतिशक्तिहीन पंगु को पर्वत को अतिक्रमण करने वाला बना सकते हैं।
हे भगवान् कृष्ण! आपने वत्स-सदृश अर्जुन तथा शुद्ध चित्त तथा भक्तिमय हृदय वाले व्यक्ति के लाभार्थ गो-सदृश उपनिषदों से समस्त ज्ञान के सार का दोहन किया।
हे भगवान् कृष्ण ! मैं आपको आत्म-निवेदन करता हूँ। ब्रह्मादि देवता आपकी कृपा तथा स्व-स्व शक्तियों के प्राप्त्यर्थ वेद-गान द्वारा आपकी पूजा करते हैं। योगी जन गहन ध्यानावस्था में निविष्ट हो आपमें तद्गत चित्त द्वारा आपका दर्शन करते हैं। आपका सत्स्वरूप न तो स्वर्ग-स्थित देवताओं को और न पाताल-स्थित दैत्यों को ज्ञात है; क्योंकि आप सबके मूल स्रोत हैं। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ।
आपने अपने वैयक्तिक आदर्श द्वारा तथा मानवता को गीता के रूप में अपनी देन के द्वारा अपने में प्रविलीन होने की प्रविधि की शिक्षा दी। कृपा कर मुझे ऐसी कुशाग्र बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं आपके उपदेशों को ग्रहण कर सकूँ तथा आपमें संविलीन हो सकूँ!
हे गीता माता! मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप गीतोपदिष्ट जीवन-यापन करने तथा सदा-सर्वदा के लिए भागवतीय चेतना की प्राप्ति में मेरे मन तथा बुद्धि का पथ-प्रदर्शन करें!
ॐ
गीता के जन्म की पृष्ठभूमि
धृतराष्ट्र और पाण्डु दो भाई थे। धृतराष्ट्र का विवाह गान्धारी के साथ हुआ था और पाण्डु के कुन्ती तथा माद्री नामक दो पत्नियाँ थीं। आखेट करते समय हुए पाप के कारण पाण्डु राजा को यह श्राप था कि वह अपनी पत्नी के साथ सम्भोग नहीं कर सकेगा। कुन्ती ने छोटी अवस्था में ऋषि की एकनिष्ठ सेवा द्वारा वरदान प्राप्त किया था, जिसके फल-स्वरूप उसको यम से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इन्द्र से अर्जुन-इस प्रकार तीन पुत्र प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार स्वर्ग के धन्वन्तरियों व अश्विनीकुमारों द्वारा माद्री से क्रमशः नकुल और सहदेव नामक दो जुड़वाँ बालक पैदा हुए थे। धृतराष्ट्र को गान्धारी से १०१ शिशु हुए थे। पाण्डु की मृत्यु के पश्चात् धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र कौरवों के साथ पाण्डुपुत्र पाँचों पाण्डवों का भी पालन-पोषण किया। पाण्डव कौरवों के साथ छोटे से बड़े हुए थे; पर पाण्डवों के शौर्य और बुद्धि-चातुर्य के कारण कौरव उन्हें अधिक समय तक अपने साथ न रख सके। अतः पाण्डवों ने राज्य के अपने आधे हिस्से में अलग रहने का निश्चय किया।
राजसूय यज्ञ के समय पाण्डवों का वैभव, सम्पत्ति और ऐश्वर्य देख कर कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन के मन में घोर ईर्ष्या और लोभ का संचार हुआ। उसने अपने मामा शकुनि की दुष्ट सलाह से युधिष्ठिर को जुआ खेलने का आमन्त्रण दे कर छल-कपट से पाण्डवों को हराया। पाण्डव जुए में द्रौपदी-सहित अपनी सारी सम्पत्ति हार गये और निर्णय हुआ कि पाण्डव द्रौपदी के साथ बारह वर्ष तक वनवास में तथा एक साल तक अज्ञातवास में रहें और तब तक दुर्योधन पूरे राज्य पर शासन करे।
कौरवों द्वारा दिये गये अनेक प्रकार के कष्ट और बाधाओं को पार करते हुए पाण्डव अपने वनवास और अज्ञातवास के तेरह वर्ष समाप्त कर पूर्व-निर्णय के अनुसार कौरवों से अपना राज्य वापस माँगने लगे; परन्तु दुर्योधन ने उन्हें एक सूई के अग्रभाग जितनी जमीन देने से भी इनकार कर दिया। तब राज्य-प्राप्ति के लिए माता कुन्ती के परामर्श एवं भगवान् श्रीकृष्ण की प्रेरणा से पाण्डवों ने कौरवों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। इस युद्ध में यादव-कुलभूषण भगवान् श्रीकृष्ण की सहायता प्राप्त करने के लिए कौरवों की ओर से दुर्योधन को तथा पाण्डवों की ओर से अर्जुन को द्वारका भेजा गया। उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण भगवान् अपने महल में पलंग पर आराम कर रहे हैं। दुर्योधन श्रीकृष्ण के शिर के पास जा कर बैठ गये और अर्जुन भगवान् के चरणों के पास खड़े रहे। श्रीकृष्ण ने जब आँखें खोली तो स्वभावतः उनकी नजर सर्व-प्रथम पैरों के पास खड़े अर्जुन पर पड़ी और बाद में पलंग के सिरहाने कुरसी पर बैठे दुर्योधन को उन्होंने देखा। श्रीकृष्ण ने उन दोनों से कुशल समाचार तथा द्वारका आने का प्रयोजन पूछा। तत्कालीन प्रथा के अनुसार प्रथम दृष्टि अर्जुन पर पड़ने के कारण श्रीकृष्ण ने पहले अर्जुन से ही प्रश्न किया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझ निःशस्त्र कृष्ण अथवा 'नारायणी-सेना' नामक मेरी समस्त शक्तिशाली सेना-इन दोनों में से किसी एक को पसन्द कर लो। श्रीकृष्ण ने यह भी चेतावनी दे दी थी कि वे स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेंगे, न शस्त्र ही धारण करेंगे। वे केवल साक्षी-रूप ही रहेंगे। यह सब स्पष्ट होने पर भी श्रीकृष्ण के सच्चे भक्त अर्जुन ने शक्ति-सम्पन्न 'नारायणी-सेना' की अपेक्षा न करके भगवान् श्रीकृष्ण को ही अपने पक्ष में लेना पसन्द किया। दुर्योधन ने अर्जुन को मूर्ख मान कर बड़ी उमंग के साथ अपने लिए शक्तिशाली नारायणी सेना की इच्छा प्रदर्शित की और श्रीकृष्ण से आश्वासन पा कर हर्षित हो हस्तिनापुर लौट आये।
श्रीकृष्ण ने जब अर्जुन से पूछा कि वे युद्ध में शस्त्र तो धारण नहीं करेंगे, फिर उनको उसने क्यों पसन्द किया? तब अर्जुन ने कहा कि भगवन् आप तो दृष्टिमात्र से ही सारी सेना का संहार करने में समर्थ हैं, फिर मुझे निःसत्त्व सेना की क्या आवश्यकता है? आप मेरे सारथि बनें, यह मेरी बहुत दिनों से हार्दिक इच्छा है। अतएव आप कृपा कर इस युद्ध में मेरी इस इच्छा की पूर्ति करें। भक्तों को हृदय से चाहने वाले प्रभु ने उसकी यह प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथि बने।
द्वारका से दुर्योधन और अर्जुन के लौट आने के बाद स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवों की ओर से मध्यस्थता करने हस्तिनापुर गये और उन्होंने युद्ध टालने का भरसक प्रयत्न किया; परन्तु अहंकारी दुर्योधन ने अपने मामा शकुनि की सलाह से शान्ति-वार्ता की उपेक्षा कर श्रीकृष्ण को बन्दी बनाने की कोशिश की। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें अपने विराट् स्वरूप का दर्शन कराया। अन्धे राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह-बन्धन के कारण उन्हें अपने काबू में नहीं रख सके और कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन ने मिथ्याभिमान से प्रेरित हो कर शक्तिशाली पाण्डवों के साथ युद्ध में सामना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया।
दोनों ओर से जब युद्ध की तैयारियाँ होने लगीं, तब मुनि वेदव्यास अन्धे धृतराष्ट्र के पास गये और कहा कि जो तुम इस भयंकर सत्यानाशी युद्ध को खुली आँखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा "हे ब्रह्मर्षियों में श्रेष मुनिवर! अपने कुटुम्बियों का संहार खुली आँखों से देखने की मेरी बिलकुल भी इच्छा नहीं है; परन्तु युद्ध का सारा विवरण सुनने की मेरी इच्छा है।" इस पर व्यास मुनि ने धृतराष्ट्र के विश्वासपात्र सलाहकार संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अन्धे राजा से कहा कि युद्ध के सारे प्रसंगों का वर्णन संजय तुम्हें सुनायेंगे। इस युद्ध में जो-कुछ होगा, उसे संजय सीधे देख सकेंगे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जान सकेंगे। उनकी आँखों के सामने या पीठ पीछे, दिन में या रात में, प्रकट-अप्रकट रूप से जो भी आचार-विचार होंगे, वे उनकी दृष्टि से छिपे नहीं रह सकेंगे। जो कुछ घटनाएँ होंगी, उनका यथार्थ चित्रण संजय के सम्मुख उपस्थित हो जायेगा। उन्हें किसी प्रकार की शस्त्र बाधा भी नहीं होगी और वह तुम्हें युद्ध का वृत्तान्त सुनाने में थकेंगे भी नहीं; पर अन्त में सत्य की ही विजय होगी।
कौरव-पाण्डवों के बीच सतत महाभारत युद्ध चलते रहने पर दश दिन के अन्त में जब महान् योद्धा भीष्मपितामह को अर्जुन ने उनके रथ से नीचे गिराया, तब संजय ने धृतराष्ट्र को यह खबर सुनायी। बाद में दुःखग्रस्त अन्धे राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पिछले दश दिनों तक लड़े गये युद्ध का सम्पूर्ण विवरण सुनाने की इच्छा व्यक्त की। बस, यहीं से भगवद्गीता का आरम्भ होता है।
विषय-सूची
3.कर्मयोग
6.ध्यानयोग
10.विभूतियोग
12.भक्तियोग
प्रथम अध्याय
अर्जुनविषादयोग
अहंकारी मन, स्वार्थ तथा आतुरता से अन्धे बने धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि उनके स्वजनों और पाण्डु के पुत्रों ने युद्ध के लिए उत्सुक हो कर धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र में क्या-क्या किया ? जहाँ वे युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, वह धर्मक्षेत्र कहलाता है, क्योंकि अग्नि, इन्द्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने वहाँ तप किया था। वह भूमि कुरुक्षेत्र भी कहलाती है; क्योंकि कौरवों के पूर्वज कुरु राजा ने भी वहाँ घोर तपश्चर्या की थी। यह मान्यता थी कि धर्मयुद्ध में जो इस भूमि पर अपने प्राण त्याग करेंगे, वे स्वर्ग में पहुँचेंगे। अतः युद्ध के लिए यह स्थान पसन्द किया गया था। संजय ने कहा कि कौरवों के राजा दुर्योधन ने पाण्डवों की सेना देखी। कौरव-सेना की तुलना में उसका संख्या-बल कम होने पर भी उसकी व्यूह रचना के कारण वह सेना विशाल दिखायी देती थी। दुर्योधन अभिमानपूर्वक अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गये। उन्हें सत्यनिष्ठ पाण्डवों के साथ युद्ध करना था। अतः अपने अन्तर के भयातुर भाव को छिपा कर वे द्रोणाचार्य को द्रुपद के साथ उनकी शत्रुता का स्मरण करा कर प्रतिकार का भाव उदीप्त करना चाहते थे; क्योंकि द्रुपद राजा के पुत्र पाण्डव-सेना की व्यूह रचना कर रहे थे। द्रोणाचार्य के शौर्य की प्रशसा इसलिए भी की गयी; क्योंकि श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम तथा पाण्डवों के पक्ष के अनेक शक्तिशाली योद्धाओं की शक्ति का उन्हें भान था। वे यह भी जानते थे कि वे स्वयं अधर्माचरण कर रहे हैं। अपने सेनापति भीष्मपितामह को उत्तेजना देने के लिए उन्होंने अन्य सभी योद्धाओं को उनकी सब ओर से रक्षा करने का आदेश दे दिया।
सबसे वयोवृद्ध एवं सेनानायक भीष्मपितामह ने युद्ध आरम्भ करने का आवाहन शंख बजा कर किया। पश्चात् कौरव-दल के अन्य योद्धाओं ने भी शंख, मृदंग, नगाड़े एवं रणभेरी के तुमुलनाद से रणक्षेत्र को गुंजा दिया। इसके पश्चात् पाण्डव-पक्ष में भी वायुपुत्र हनुमान् की आकृति से अंकित ध्वजा फहराते श्वेत अश्वों से युक्त सुसज्जित रथ में बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन तथा अन्य योद्धाओं ने अपने दिव्य शक्तिशाली शखों की प्रचण्ड ध्वनि से कौरवों के युद्ध के आवाहन का प्रत्युत्तर दिया। उनकी गर्जना से आकाश और पृथ्वी ही निनादित नहीं हुई, अपितु समस्त कौरव-सेना के हृदय में भय का संचार हुआ।
धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध-कार्य के लिए अवस्थित देख कर योद्धाओं के दर्शन हेतु अर्जुन ने श्रीकृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ला कर खड़ा करने को कहा। श्रीकृष्ण ने रथ जहाँ भीष्म, द्रोण तथा अन्य महान् योद्धा खड़े थे, वहाँ ला कर खड़ा किया। विदुर जी ने युद्ध से होने वाले जिन अनिष्टों का वर्णन किया था, अपने गुरुजनों और सगे-सम्बन्धियों को देख कर, उनकी याद अर्जुन के मन में ताजी हुई। पाण्डवों को हताश करने के लिए शकुनि को एक कपट-युक्ति सूझी। उसने पाण्डवों के प्रति अत्यन्त सहृदय आदर-भाव रखने वाले विदुर जी से जा कर कहा कि वे पाण्डवों के पास जा कर उन्हें समझायें कि युद्ध के क्या अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। फलतः इस युद्ध के द्वारा उनके ही गुरु एवं सम्बन्धी-जनों की हत्या का पाप, अनेक स्त्रियों के पति-मरण से विधवा होने की शक्यता एवं उससे दुराचार, व्यभिचार के प्रसार की सम्भावना, राष्ट्र की सम्पत्ति और वैभव का विनाश, घोड़े, हाथी आदि निर्दोष प्राणियों का संहार आदि के सम्बन्ध में विदुर जी ने अर्जुन को सब बातें बतलायीं। इस परामर्श को स्मरण कर अर्जुन बहुत दुःखी हुए और उन्होंने युद्ध से इनकार किया।
अपने गुरुओं और सगे-सम्बन्धियों को मारे बिना राज्य करने की इच्छा प्रदर्शित करने के स्थान में अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को भूल कर श्रीकृष्ण से कहने लगे कि उनके हाथ में गाण्डीव धनुष को पकड़ कर रखने तक की शक्ति नहीं रह गयी है तथा युद्ध में उनके पराजय के अपशकुन भी उन्हें दिखायी देने लगे हैं। अपने गुरुजनों की हत्या के भव से चिन्तित एवं भगवान् श्रीकृष्ण की शक्ति से अपरिचित अर्जुन विद्वान् के समान युद्ध के अनिष्ट परिणामों का वर्णन करते हुए कहने लगे कि गुरुओं एवं सगे-सम्बन्धियों को मार कर वे राज्य का आनन्द भोगना नहीं चाहते और इस युद्ध द्वारा यदि तीनों लोकों का राज्य भी उन्हें मिलता हो तो भी उसकी उन्हें चाह नहीं है। अर्जुन यह मानते हैं कि सगे-सम्बन्धियों की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य का उपभोग करने की अपेक्षा मोह के वशीभूत हुए कौरव ही उन्हें मार डालें तो अच्छा है। श्रीकृष्ण की सर्वज्ञ शक्ति को भूल कर वे माया और शोक से पीड़ित हो कर यह तर्क करते हैं कि कुटुम्ब के नाश से कुल-परम्परागत सनातन धार्मिक विधियों का नाश होगा, स्त्रियाँ व्यभिचारिणी बनेंगी, जिससे वर्णसंकरता होगी तथा आप्तजनों के नाश करने से नरक-वास भोगना पड़ेगा। अर्जुन यह सोचते हैं कि वे स्वयं नि शस्त्र और प्रतिकार-रहित हो कर युद्ध में खड़े रहे और कौरव उन्हें मार डालें। यही श्रेयस्कर है। इस प्रकार अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए शोकमग्न अर्जुन अपने धनुष-बाण को एक ओर छोड़ कर रथ पर विषण्ण अन्त करण से बैठ गये।
इस अध्याय में मनुष्य को निम्नांकित उपदेश मिलते हैं धृतराष्ट्र के समान जब मनुष्य का मन मोह और स्वार्थ से अन्धा हो जाता है, तब वह राष्ट्रहित की परवाह नहीं करता और परिणाम स्वरूप अपने ही आप्तजनों एवं समस्त राष्ट्र के विनाश का कारण बनता है।
दुर्योधन के समान मन जब अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, कपट, अहंकार, कीर्ति की इच्छा तथा नाम और सत्ता की कामना से अभिभूत होता है, तब मनुष्य अपने मित्रों तथा सगे-सम्बन्धियों एवं प्रजा का नाश करने में नहीं हिचकिचाता और अन्ततः वह अपना ही नाश कर लेता है।
अर्जुन के समान मनुष्य जब मोह और कामनाओं से ग्रसित हो, स्वधर्म-पालन में निष्फल होता है, तब वह अपने बल एवं साहस को खो बैठता है और श्रीकृष्ण जैसे प्रभु के सम्मुख होते हुए भी भगवान् की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाता।
संजय के समान मनुष्य जब सहृदयी, ईश्वर-भक्त, स्वामी भक्त और निष्काम हो कर शत्रु एवं मित्र के प्रति समान भाव रखता है, तब उसे मानसिक शान्ति प्राप्त हो कर ईश्वर के विश्व-रूप का दर्शन होता है।
इस अध्याय में यह समझाया गया है कि द्वन्द्व ही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। अर्जुन के व्यक्तित्व के दुविधायुक्त चारित्र्य, उसके मन और हृदय एवं विचार और लगन के बीच की विसंवादिता के कारण ही ऊपर वर्णन की गयी आपत्तियाँ उपस्थित हुई हैं। एक ओर जहाँ पापी शत्रुओं का नाश करने के लिए उनका क्षत्रिय धर्म उन्हें प्रेरित करता है, वहीं दूसरी ओर अपने सगे-सम्बन्धियों तथा गुरुजनों के स्नेह एवं प्रेम के लिए उनका हृदय छटपटाता है; अतः उनके विनाश का निमित्त बनने से वे बचना चाहते हैं। इस प्रकार की आन्तरिक विसंवादिताएँ अर्जुन के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एव आध्यात्मिक स्तरों को असन्तुलित बना कर उनके मन में विषाद उत्पन्न करती हैं।
इस प्रकार 'अर्जुनविषादयोग' नामक यह प्रथम अध्याय समाप्त होता है।
द्वितीय अध्याय
सांख्ययोग
मोह और भय से व्यग्र हुए अर्जुन की परिस्थिति का संजय वर्णन करते हैं। अपना आशय स्पष्ट रूप से प्रकट करने के स्थान में अर्जुन दम्भ से कुटुम्ब के प्रति कर्तव्य, युद्ध से होने वाले दोष, पूज्य द्रोणाचार्य एवं भीष्मपितामह की हत्या आदि की बातें करते हैं। श्रीकृष्ण के सन्तोष के लिए वे त्याग की भावना और भिक्षा माँग कर जीवन-निर्वाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं।
अर्जुन की इस स्थिति को देख कर भगवान् श्रीकृष्ण उनके विषादपूर्ण हृदयदौर्बल्य के लिए उनकी भर्त्सना करते हैं और उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मन में जब विरोधी विचार उठते हैं, तब मनुष्य किंकर्तव्यविमूढ़ बन जाता है। ऐसे समय पर मनुष्य को किसी ज्ञानी पुरुष अथवा गुरु का परामर्श आवश्यक होता है। बारम्बार संसार के थपेड़े खा कर मनुष्य का अहंभाव अपनी असमर्थता एवं असहायता का अनुभव करता है और तब शान्ति की आशा से सर्वशक्तिमान् प्रभु की ओर मुड़ता है, उसकी शरण में जाता है। अर्जुन भी अपनी काल्पनिक विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता के अहंकारपूर्ण विचारों से श्रीकृष्ण को निश्चय कराने में असफल सिद्ध हुए, तब उन्हें अपनी निर्बलता का भान हो गया और वह अनन्य भाव से श्रीकृष्ण की शरण में जा कर उनके आश्रित बन गये, सच्चे अर्थ में उनके वह शिष्य बन गये। अपने मन की उलझन पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान् श्रीकृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। तब मुस्कराते हुए श्रीकृष्ण अर्जुन के अज्ञान और काल्पनिक भय को दूर करते हैं। अर्जुन की उत्सुकता, सहृदयता, निःस्वार्थ शरणागति और आत्मज्ञानाभाव को देखते हुए उन्हें प्रथम 'सांख्ययोग' अर्थात् आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं और उसके पश्चात् जीवन के अन्तिम उद्देश्य अर्थात् परम साक्षात्कार को प्राप्त करने के मार्ग 'कर्मयोग' का उपदेश देते हैं। वे आत्मा के अविनाशी स्वभाव के विषय में शिक्षा देते हुए कहते हैं कि आत्मा के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ नहीं है। वह त्रिकालाबाधित है। अर्जुन की मर्यादित बुद्धि को ध्यान में रखते हुए भगवान् श्रीकृष्ण बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था के शारीरिक परिवर्तनों का उदाहरण दे कर समझाते हैं कि इन परिवर्तनों के कारण जैसे व्यक्ति का 'मैं'-पन नहीं बदलता, वैसे ही जन्म-मरण आदि के कारण भी आत्मा में कोई फेर-बदल नहीं होता। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को छोड़ कर मनुष्य नये वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीव पुराना शरीर छोड़ कर नये शरीर को ग्रहण कर लेता है। जिन-जिन इच्छाओं की तृप्ति के लिए जीव इस संसार में जन्म लेता है, उनका अनुभव लेने के बाद वह शरीर त्याग देता है।
इन्द्रियों के साथ विषयों के सम्पर्क से प्रत्येक व्यक्ति सुख-दुःख, शीत-उष्ण आदि का अनुभव करता है। इन्द्रियाँ नाड़ियों के माध्यम से अपनी अनुभूति को मन तक पहुँचाती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह योग साधना द्वारा इन्द्रियों को कछुए के समान समेट कर उन्हें विषयों से खींच ले और मन को सन्तुलित रखे। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में सुख और दुःख को समान मानने की क्षमता है, वही अमरता को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। आत्मा अविकारी और सत् है। अन्य जो विकारी वस्तुएँ हैं, वे सब असत् हैं। इस अविनाशी आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। व्यक्ति जो जब यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा का जन्म-मरण नहीं है, तब वह इस नाशवान् शरीर के नष्ट होने पर कभी शोक नहीं करता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश- इन पंचमहाभूतों के परे जो आत्मा है, उसको न शस्त्र काट सकते हैं, न वह जल से भीगता है, न उसे अग्नि जला सकती है और न उसे वायु ही सुखा सकती है। वह सर्वव्यापी, शाश्वत, अविकारी और अविचल है। श्रीकृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह जिन शक्तिशाली शस्त्रों से अपने सगे-सम्बन्धियों को मारने का विचार कर रहा है, वे किसी को मार डालने में असमर्थ हैं। आत्मा का बुद्धि द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता और न उसे जाना जा सकता है। वह इन्द्रियग्राह्य भी नहीं है; क्योंकि वह इन्द्रियों की पहुँच से सर्वथा परे है।
भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन के विक्षिप्त मन को समझाने के लिए युद्ध के भौतिक लाभों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि क्षत्रिय का सुख पारिवारिक आनन्द या भौतिक भोगों में नहीं; अपितु धर्मस्थापना हेतु सत्य एवं न्याय के संग्राम करने में है। श्रीकृष्ण कहते हैं, "यदि तुम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो वसुन्धरा पर सुखपूर्वक राज्य कर सकोगे और यदि युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो गयी तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तुमने इस समय युद्ध करने के अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, तो तुम्हें अपने स्वजनों द्वारा ही अपमानित होना पड़ेगा, जो कि मृत्यु से भी अधिक दुःखदायी एवं लज्जाजनक है। परिणाम की आशा न रखते हुए सुख एवं दुःख में मन का सन्तुलन बनाये रख कर यदि तुम कर्तव्य-भावना से युद्ध में प्रवृत्त होगे, तो तुम्हें कदापि पाप नहीं लगेगा।"
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्रारम्भ में 'सांख्ययोग' का उपदेश दिया और तत्पश्चात् निःस्वार्थ सेवा का मार्ग अर्थात् फलाकांक्षा छोड़ कर कर्म करने की कला- 'कर्मयोग' सिखाया। श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म आ जायें वे स्वागत योग्य हैं, यदि उन्हें सन्तुलित मन से कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया जाये। जब हम किसी कार्य के फल की इच्छा नहीं रखते, तब कर्म करते समय मन शान्त रहता है। ज्ञानी की एकाग्र बुद्धि का कारण उसकी निष्काम वृत्ति ही है तथा अज्ञानी की विचलित बुद्धि का कारण कामना है। बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा ही अमरता प्राप्त करने की आशा की जा सकती है।
श्रीकृष्ण इस अध्याय में जिसका मन सन्तुलित एवं निःस्वार्थ है ऐसे कार्यरत कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं और अर्जुन को युद्ध के प्रसंग में भी वैसे भी बनने का आदेश देते हैं। वे अर्जुन को राज्य की प्राप्ति अथवा उसके संरक्षण की कामना से रहित हो युद्ध करने का परामर्श देते हैं। इस प्रकार व्यक्ति प्रकृति के सत्त्व, रज और तमस् नामक तीन गुणों से परे हो कर अपनी आत्मा में स्थित होता है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, वह जानता है कि तीनों लोकों में प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है। इसलिए जय-पराजय, हानि-लाभ आदि में व्यक्ति का मन सन्तुलित रहना चाहिए। इसी को योग कहते हैं। मोह-रहित हो कर हर समय मन को सन्तुलित रखते हुए कर्म करना 'कर्मकौशल' कहलाता है। मन का सन्तुलन रखने से व्यक्ति शुभ और अशुभ-दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग कर परम चैतन्य अर्थात् आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर करता है। यह सब सुन कर अर्जुन स्थिर मन वाले (स्थित-प्रज्ञ) मनुष्य के विषय में चार प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे मनुष्य की परिभाषा क्या है तथा वह कैसे बोलता, बैठता और चलता है? श्रीकृष्ण कहते हैं कि स्थित-प्रज्ञ मनुष्य की कोई आकांक्षा नहीं होती। वह आत्मज्ञान और वासना-क्षय का एक-साथ अनुभव करता है। जब मन में कोई वासना नहीं होती, तब उसके परिणाम-स्वरूप होने वाले भय और क्रोध जैसे दूषण भी उसमें नहीं रहते, उनका अपने-आप नाश हो जाता है। भगवान् कहते हैं कि जिस पुरुष में ज्ञानोदय हो जाता है. वह तात्कालिक परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। उसमें राग, द्वेष नहीं होते। वह जगत् का न तो आलिंगन करता है और न उससे घृणा ही करता है, अपितु कछुए के समान अपनी इन्द्रियों को समेट कर उन्हें अन्तर्मुखी बना लेता है। सबमें परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला अपनी इन्द्रियों पर अधिकार पा लेता है। श्रीकृष्ण अनियन्त्रित मन की आँधी में फँसी हुई नौका से तुलना करते हैं। वासना की वायु का झौंका आते ही मन डाँवाडोल हो जाता है और बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सामान्य मनुष्य की अँधेरी रात जितेन्द्रिय मनुष्य के लिए जाग्रत अवस्था के समान है। इसके विपरीत सामान्य मनुष्य का दिन जितेन्द्रिय मनुष्य के लिए रात्रि के समान है। स्थित-प्रज्ञ योगी के विश्वात्म-भाव में सारी विशिष्टताएँ विलीन हो जाती हैं। स्थित प्रज्ञ योगी अनासक्त सेवामय जीवन बिताता है।
इस अध्याय में समझाये गये सांख्य-शास्त्र में भारतीय षड्दर्शनों के मूलभूत सिद्धान्तों का समावेश किया गया है। भगवद्गीता का योग मनुष्य को अपने दैनन्दिन जीवन में उसे किस प्रकार उतारा जाये, इसकी शिक्षा देता है। भगवान् जीवन का विस्तृत ज्ञान देते हैं, जिसको हृदयंगम करने से अनन्त की अनुभूति के साथ मानव के समस्त दुःख दूर हो सकते हैं।
इस अध्याय में भगवान् मानव को द्वन्द्व से परे होने का मार्ग एवं संघर्षों पर विजय पाने की वैज्ञानिक पद्धति बतलाते हैं। वे कहते हैं- 'साक्षी बन कर रहो', त्रिगुणातीत बनो', 'द्वन्द्व से परे हो कर अहंभाव को छोड़ कर जिओ', 'फल की आशा किये बिना कर्म करो', 'परम सत् के साथ अपना ऐक्य समझ कर कर्म करो' आदि-आदि। जिसे आत्म-साक्षात्कार हो गया है, ऐसे स्थित-प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बता कर भगवान् श्रीकृष्ण मनुष्य की मिथ्या धारणाओं को दूर करते एवं उद्विकास की सभी श्रेणियों तथा प्रक्रमों में सम्भाव्य मोक्ष-प्राप्ति की प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करते हैं।
इस प्रकार यह 'सांख्ययोग' नामक द्वितीय अध्याय समाप्त होता है।
तृतीय अध्याय
कर्मयोग
पिछले अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण ने यह उपदेश दिया था कि सन्तुलित मन से किया हुआ कर्म 'बुद्धियोग' है। फल की आशा से किया हुआ कर्म 'बुद्धियोग' से बहुत निम्न कोटि का कर्म है। अर्जुन इसका अर्थ नहीं समझ सके। उन्होंने समझा कि बुद्धि और कर्म-ये दो शब्द क्रमशः ज्ञान और कर्म-मार्ग के प्रतीक हैं। अतः उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा कि 'क्या आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठतर समझते हैं? और यदि ऐसा है तो फिर मुझे आप इस भयंकर कर्म, युद्ध के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? क्या करने से परम कल्याण हो सकता है, कृपया समझायें।' तब श्रीकृष्ण सविस्तार उन्हें समझाते हैं। वे कहते हैं कि विद्या और अविद्या के समन्वय से 'कर्मयोग' का आचरण करना चाहिए। अहन्ता-सहित चेतना विद्या है और अहन्ता-रहित अज्ञान अविद्या है। इन दोनों के सत्-पक्ष का संयोग अर्थात् अहंकार-रहित चैतन्य 'कर्मयोग' कहलाता है। पिछले अध्यायों में भगवान् श्रीकृष्ण ने सांख्ययोग और कर्मयोग नामक दो मार्गों का वर्णन किया है। इस अध्याय में वे कर्मयोग का विश्लेषण करते हैं तथा दैनिक जीवन में उसका व्यावहारिक उपयोग बतलाते हैं। कर्म-संन्यास द्वारा कोई भी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि उसका मन गुप्त रूप से अन्दर कार्य करता रहता है। प्रकृति के तीनों गुण-सत्त्व, रज और तम शरीर, मन और बुद्धि-सहित संसार की प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और इस कारण कोई भी मनुष्य सदैव शान्त नहीं रह सकता। जो मनुष्य बाह्याचार में इन्द्रियों का निरोध कर कर्म-संन्यास करता है और दूसरा कोई न देखे, इस प्रकार भीतर-ही-भीतर कामनाओं में विचरता है, वह दम्भी है। दूसरी ओर जो व्यक्ति भीतर से आत्मा के विषय में मनन-चिन्तन करता है और परिणाम एवं फल की आशा न रखते हुए बाहर से कर्म करता है, वह कर्मयोगी है। कोई भी कर्म-संन्यासी बन कर अपने शरीर तक का निर्वाह भी नहीं कर सकता; क्योंकि श्वासोच्छ्वास लेना, देखना, सुनना, भोजन करना, पचाना आदि सभी व्यवहार भी तो क्रिया ही हैं। श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्तापन का अभिमान छोड़ कर कर्म करने के लिए समझाते हैं। जगत् स्वयं कर्म से बँधा हुआ है। स्वार्थ-भावना-रहित किया गया कर्म यज्ञ-स्वरूप है। जो व्यक्ति इस यज्ञ-भावना से कर्म करता है, उसका हृदय निर्मल होता है और वह ईश्वर-साक्षात्कार की ओर उन्मुख हो जाता है। इसलिए श्रीकृष्ण अर्जुन को किसी भी प्रकार की कामना न रखते हुए कर्तव्य-भावना से यज्ञ (कर्म) करने का उपदेश देते हैं।
सार्वजनिक उद्देश्य से प्रेरित हो कर किया गया सहेतुक कर्म कर्मयोग है। कर्म ईश्वर की पूजा है, ऐसा समझ कर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब पूजा की भावना से विचारपूर्वक कर्म किया जाता है, तब वह युगपत् कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग बन जाता है। इसलिए जिस प्रकार वर्षा, सूर्य, वृक्ष आदि समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ-रूप कर्म अविरत करते रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रीकृष्ण राजा जनक तथा अन्य महापुरुषों का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने कर्म द्वारा पूर्णता प्राप्त की थी। यहाँ भगवान् अर्जुन को अन्य योद्धाओं का नेतृत्व करने के उनके उत्तरदायित्व का भान कराते हैं; क्योंकि वे सब उनके साहस और शास्त्र-निपुणता पर निर्भर थे। यहाँ तीनों लोकों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए फलाकांक्षा-रहित हो कर कर्म करने का रहस्य श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं तीनों लोकों के विषय में सब-कुछ जानते हैं। अर्जुन के मन की बात जानने की शक्ति भी उनमें है। श्रीकृष्ण अर्जुन के दम्भपूर्ण भाव की अप्रत्यक्ष रूप से निन्दा करते हैं। अर्जुन को भली-भाँति समझ में आ जाये, इस प्रकार श्रीकृष्ण युद्ध में उनकी स्वयं की भूमिका और दृष्टिकोण को उद्धृत करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि स्वयं कर्म का त्याग कर अथवा दूसरों को इस प्रकार की शिक्षा दे कर उनको अपने धर्म के पालन-रूप कर्म से उपरत न करे। ऐसे व्यक्ति को स्वय मार्गदर्शक एव उदाहरण-स्वरूप बन कर दूसरों का नेतृत्व करना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञानयुक्त मार्गदर्शन मिलने पर समस्त संसार ज्ञानी का अनुकरण करने लगेगा। कर्तापन की भावना के सम्बन्ध में अर्जुन की मनोवृत्ति की पुन भर्त्सना करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुण बाह्य वस्तुओं के गुणों पर प्रभाव डालते हैं और अन्तत यह तथ्य ही कर्म का रहस्य है।
मानव-शरीर प्रकृति-जनित है। सत्त्वगुण की प्रधानता से व्यक्ति शुभाशुभ कर्मों के भेद को जान सकता है। व्यक्ति प्रकृति के सब गुणों का साक्षी भी बन सकता है। रजोगुण की प्रबलता से व्यक्ति अपने को शरीर मान लेता है और स्वयं कर्ता की तरह व्यवहार करता तथा अनुभव करता है जिसके फल-स्वरूप वह संसार में बंध जाता है। तमोगुण की वृद्धि से व्यक्ति अज्ञानी जड़ और प्रमादी बन जाता है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि इन्द्रियों के गुण अन्दर से क्रिया करते हुए बाह्य विषयों के गुणों का अनुसरण करते हैं। अतः ऐसे पुरुष उन विषयों से इन्द्रियों को हटा कर उन्हें अन्तर्मुख करते हुए आत्मा का मनन-चिन्तन करते हैं।
श्रीकृष्ण अर्जुन को विचार, वाणी और कर्म से सब-कुछ भगवान् को समर्पण कर एवं शरीर को ईश्वर का उपकरण मान कर कर्म करने की व्यावहारिक युक्ति बतलाते हैं। व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य-पालन में असफल होता है, तो वह अपना नाश कर लेता है। इन्द्रियों का विषयों के प्रति राग और द्वेष-दोनों अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। हम विवेक और आत्म-समर्पण द्वारा उनसे परे हो सकते हैं। मानव के गुणों का विश्लेषण करते हुए श्रीकृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य से विमुख होने के बदले युद्ध करने का अनुरोध करते हैं। स्वधर्म-पालन में भय या रुकावटें हों तो भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ऐसा करते हुए कदाचित् मृत्यु भी आ जाये, तो वह भी कल्याणकारक है। स्वधर्म त्याग कर दूसरों का धर्म ग्रहण करने पर सम्भव है मान, सत्ता एवं प्रतिष्ठा मिले; पर अन्ततोगत्वा उससे भय, अशान्ति और दुःख ही उपलब्ध होंगे, इसलिए स्वधर्म का पालन करना ही श्रेयस्कर है।
अर्जुन श्रीकृष्ण से पूछते हैं कि व्यक्ति अपने श्रेय के विपरीत आचरण क्यों करता है और उसे पाप-कर्म करने के लिए कौन प्रेरित करता है? श्रीकृष्ण बतलाते हैं कि व्यक्ति आकांक्षा एवं कामना के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप-कर्म करने को प्रवृत्त होता है। मन, बुद्धि और इन्द्रियों में इच्छा का वास है। जैसे धुएँ से अग्नि, धूल से दर्पण एव जेर से गर्भ आच्छादित हो जाता है, वैसे ही कामना से ज्ञान बँक जाता है। मानव सुख खोजता है; पर राजसिक इच्छा और अज्ञान के कारण वह उसे इन्द्रियों द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करता है जिसके परिणाम स्वरूप वह पापमय कर्म तथा विनाश की ओर अग्रसर होता है। अप्रशिक्षित घोड़ों के समान इन्द्रियाँ शरीर-रूपी रथ को कुमार्ग पर खींच कर ले जाती हैं।
शरीर से परे इन्द्रियाँ हैं और इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा है। इस प्रकार समझ कर कि शरीरान्तर्वासी आत्मा शुद्ध चैतन्य-रूप है और वह (आत्मा) शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि से परे तथा कर्म से अलिप्त है श्रीकृष्ण कहते हैं कि इन्द्रिय, मन और बुद्धि काम के वास-स्थान हैं। वे अर्जुन को कहते हैं कि मन और बुद्धि का शुद्धात्मा के साथ तादात्म्य न करें। उनके मान्यतानुसार कामनाओं से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। अज्ञान के कारण मनुष्य कामनाओं का दास बनता है और विषयेन्द्रियों द्वारा कामनाएँ तृप्त करता है; परन्तु वह अन्तरात्मा की सत्यता को पहचानने में असमर्थ रहता है। योग-साधन के मध्यम मार्ग के अनुसरण, अन्तर्निरीक्षण द्वारा चित्तवृत्तियों का दैनिक विश्लेषण तथा ध्यान के अभ्यास द्वारा मनुष्य गुरु के मार्गदर्शन एवं ईश्वर की कृपा से आत्म-साक्षात्कार कर लेता है।
इस अध्याय में मानव को यह शिक्षा दी गयी है कि कर्म किये बिना जीना असम्भव है। अतः पिछले अध्याय में बताये नियमानुसार 'योगस्थः कुरु' (योगारूढ़ हो कर) कर्म करना चाहिए। भगवान् राजा जनक का उदाहरण देते हुए उनका अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। 'कर्म' विविधता और क्रिया का क्षेत्र है तथा विविधता के क्षेत्र में रह कर भी दिव्यता के साथ एकता-स्थापन 'योग' है। शक्ति के मूल-स्रोत का ध्यान रखते हुए कर्म करना चाहिए। मन जब इन्द्रियों के कारण बहिर्मुखी हो जाता है, तब अनेक मानवी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। मन सुख की खोज करता है और यही उसका स्वरूप भी है; परन्तु अज्ञान के कारण वह इन्द्रियों द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहता है और विषयों में लिप्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि मन अपने मूल स्रोत परम चैतन्य आत्मा की ओर उन्मुख हो जाये, तो वह अवर्णनीय सुख प्राप्त कर सकता है। विचार (व्यक्ति चैतन्य) रहित मानव ईश्वर है और व्यक्ति चैतन्य सहित ईश्वर मानव बन जाता है।
भगवान् हमें सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणों से परे होने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि बुद्धि, मन और इन्द्रियों की प्रक्रियाओं से हमें सदैव सचेत एवं जाग्रत रहना चाहिए। बुद्धि के स्तर तक ही इच्छाओं का निवास है। जब बुद्धि और मन अन्तर्चेतना के साथ एकरूप हो जाते हैं, तब समुद्र में विलीन हुई लहर के समान इच्छाएँ अपने-आप ही अपना बल खो बैठती हैं।
इस प्रकार यह 'कर्मयोग' नामक तृतीय अध्याय समाप्त होता है।
चतुर्थ अध्याय
ज्ञानविज्ञानयोग
दैनिक जीवन में कर्मयोग के आचरण की विधि एवं विवरण बताने के पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने प्रथम सूर्य को सिखाया था। तदनन्तर मनु, इक्ष्वाकु आदि सूर्यवंश के राजाओं को वंश-परम्परा से यह प्राप्त हुआ था। इन राजर्षियों ने इस योग का अभ्यास कर इसका जन-साधारण में प्रचार किया। बाद में इन महारथियों के अभाव में कालान्तर में सामान्य जनता में इस योग की महत्ता का क्रमशः हास हुआ था। श्रीकृष्ण को सर्वज्ञ होने के कारण भूत, वर्तमान और भविष्य-त्रिकाल का ज्ञान था, जब कि अर्जुन अपने जीव-भाव के कारण अपना भूतकाल भूल गये थे। भगवान् श्रीकृष्ण अपने जन्म का रहस्योद्घाटन करते हैं। वे कहते हैं कि साधु-पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने एवं प्रकृति को नियन्त्रित रखने के लिए योगमाया (दैवी शक्ति) द्वारा वे अवतार लेते हैं। अपने आदर्श द्वारा मानवता के उद्धार के लिए ईश्वर अवतरित होते हैं। अर्जुन के हृदय की पवित्रता, उनके विचार, वाणी और कर्म के समर्पण तथा सत्य का साक्षात्कार करने की उनकी उत्कण्ठा देख कर श्रीकृष्ण उन्हें योग का रहस्य समझाते हैं। भगवान् कहते हैं कि वे स्वयं बिना किसी पक्षपात के मानव जाति की इच्छा के अनुसार उसकी आवश्यकता को पूरी करते हैं। मानवता के उद्विकास की प्रक्रिया में मानव-स्वभाव के स्तर के अनुसार इच्छाओं में भिन्नता होती है। अतः गुण और कर्म के अनुरूप उसके चार वर्ण बनाये गये हैं। जिनमें शम, दम, आर्जव, गाम्भीर्य तथा शात्र-ज्ञान है और जो दूसरों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति सत्त्वगुण-प्रधान होते हैं। जो शौर्य, तेज, धैर्य, कुशलता, उदारता, प्रभुता आदि गुणों से विभूषित होते हैं और जिनमें राज्य करने की क्षमता होती है, वे क्षत्रिय कहलाते हैं। इनमें राजस गुण की प्रधानता होती है। जो लोग कृषि, पशु-पालन तथा वाणिज्य-व्यापार आदि करते हैं और जिनमें रजोगुण के अधीन तमोगुण भी रहता है, वे वैश्य कहलाते हैं और जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण तमोगुण के अधीनस्थ होता है, वे अन्य तीनों वर्णों की सेवा करते हैं तथा शूद्र कहलाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने फल की अपेक्षा न रखते हुए गुण एवं स्वभाव के अनुसार स्वधर्म का आचरण करे तो वह ईश्वर को पा सकता है। जिसमें ब्रह्मज्ञान है, वह ब्राह्मण कहलाता है। कोई भी वर्ण वंश-परम्परा अथवा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है।
अवतार के प्रयोजन तथा इच्छा-विहीन अस्तित्व का निरूपण करते हुए श्रीकृष्ण अर्जुन को फलेच्छा-रहित हो कर्म करने का उपदेश देते हैं। कर्मयोग द्वारा सब बन्धनों से मुक्त हुआ जा सकता है। वे समझाते हैं कि प्राचीन मुमुक्षु पुरुषों ने इस प्रकार का निःस्वार्थ कर्म किया था; अतः वे अर्जुन से इसी भाँति कर्म करने तथा मोह या भय से अपने धर्म का त्याग न करने का उपदेश करते हैं।
श्रीकृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपना धर्म निश्चित करना बड़ा दुष्कर कार्य है। अतः स्वधर्म का पालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, यह जान लेना आवश्यक है। पूर्वगामी अध्याय में यह समझाया गया है कि कर्म किये बिना कोई शान्त नहीं बैठ सकता। अब यहाँ वे बतलाते हैं कि हमें कर्म, अकर्म और अकर्म में कर्म का रहस्य जान लेना चाहिए। शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि द्वारा जो क्रिया की जाती है, वह कर्म कहलाता है। नियमानुसार अपने धर्मानुकूल फलाशा छोड़ कर मोह, अहन्ता एवं ममता को त्याग कर यदि कोई कर्म किया जाये तो वह कर्म में अकर्म हो जाता है। ऐसा अनासक्त कर्म करने वाला पुरुष मनुष्यों में सचमुच ज्ञानी तथा योगी है। सामान्य रूप से अकर्म का अर्थ सभी शारीरिक क्रियाएँ छोड़ देना होता है; पर बाह्य क्रियाएँ छोड़ कर नाम और कीर्ति के लिए जो त्यागी बनने का ढोंग करता है, वह पाप और बन्धन का भागी होता है। जो कोई शरीर द्वारा कोई कर्म किये बिना शान्त बैठा रहता है, पर मन से कर्म करता रहता है, कामना करता है, वह कर्म ही करता है और इसे अकर्म में कर्म कहते हैं। जो यह भेद समझते हैं, वे अपने प्राप्त वर्णाश्रमानुसार कर्तव्यों को शारीरिक दुःख के भय से नहीं त्यागते।
जो पुरुष अन्तःकरण में परमात्मा का चिन्तन करता है और नि स्वार्थ भाव से फलाशा छोड़ कर संसार की भलाई के लिए ज्ञानपूर्वक कर्म करता है, उसे ज्ञानी लोग कर्म में अकर्म का ज्ञाता एवं पण्डित कहते हैं। इस प्रकार के कर्म में अकर्म से सभी पाप दग्ध हो जाते हैं। वह जन्म-मरण के बन्धनों से छूट जाता है। वह संसार से किसी बात की अपेक्षा अथवा इच्छा नहीं करता और सदा सुखी बना रहता है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में सम भाव रखता है। शास्त्रों में वर्णित सभी प्रकार के यज्ञ-कर्म करता है। ऐसा पुरुष ज्ञानी अथवा ब्रह्म-स्वरूप हो जाता है।
दूसरे अध्याय में श्रीकृष्ण भगवान् ने बतलाया कि आत्मा अथवा ब्रह्म सर्वव्यापक है। जो कोई प्रत्येक कर्म में ब्रह्म का अनुभव करता है, वह ब्रह्म को ही कर्ता, कर्म और कर्म-फल मानता है। इसे 'ज्ञान-यज्ञ' कहते हैं। श्रीकृष्ण स्वाध्याय, इन्द्रिय-निग्रह, प्राणायाम, दान आदि यज्ञ के विविध रूपों का वर्णन करते हैं। ये सारे यज्ञ-कर्म शरीर, मन और इन्द्रियों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। इन यज्ञों को न करने वाला व्यक्ति ऐहिक तथा आध्यात्मिक सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। फल की आशा से दान, पवित्र अग्नि में अममा चार-सहित घी, चावल आदि हवन-सामग्री की आहुतियों द्वारा किये यज्ञादि से ऐहिक सुख भले ही प्राप्त हो जाये, पर इस प्रकार अज्ञान से किये गये सकाम-यज्ञ से फलाशा-रहित किया जाने वाला ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ है। जिस प्रकार प्रज्वलित अधि काष्ठ-समुदाय को भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञानानि पाप-समूह को विदग्ध कर डालती है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि सद्भावना से, चित्त-शुद्धि से, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की भक्तिपूर्वक सेवा से, कर्मयोग के सतत दीर्घकालीन आचरण से एवं इन्द्रिय-निग्रह से यह ज्ञान प्राप्त होता है।
श्रीकृष्ण कहते हैं कि आत्मा अर्थात् सत्ता (अन्तरस्थ शुद्ध चैतन्य) का भान ही सच्चा ज्ञान है। दीर्घ काल तक गम्भीर ध्यान का अभ्यास करने से साधक इस शुद्ध चैतन्य का अनुभव कर सकता है। इसके लिए ईश्वर में अपार श्रद्धा, गुरु में विश्वास, धैर्य, समर्पण की भावना के साथ सांसारिक विषयों से प्रयत्नपूर्वक इन्द्रियों की निवृत्ति आवश्यक है। ऐसा होने पर व्यक्ति को परम शान्ति का लाभ हो सकता है। अज्ञानी मूढ़ जन इन गुणों के अभाव में अपने-आपमें तथा दूसरों के प्रति शंकाशील होते हैं और इस लोक तथा परलोक में दुःखी रहते हैं; परन्तु जो लोग कर्मों का त्याग कर किसी प्रकार की कामना न रखते हुए सहज भाव से ज्ञानपूर्वक ध्यानयोग की साधना करते हैं, उन्हें संसार की कोई शक्ति बन्धन में नहीं डाल सकती। जिसके द्वारा अर्जुन के पूर्वजों ने मानव-जीवन का चरम उद्देश्य-परमानन्द प्राप्त किया था, उसी कर्मयोग का अनुसरण करने के लिए श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं।
इस अध्याय में भगवान् ने यह बताया है कि व्यक्ति को इस बात का सदा भान रहना चाहिए कि आत्मा कर्म तथा अकर्म-दोनों ही अवस्थाओं में असंग तथा अलिप्त रहता है। इस प्रकार समष्टि (ब्रह्म) तथा व्यष्टि (जीव) चेतना की स्थिति में त्याग अथवा असंग भाव स्वाभाविक ही रहता है। ब्रह्माण्डीय स्तर की अवस्था में सर्वशक्तिमान् प्रभु सृष्टि के सृजन, पालन तथा विनाश के समय केवल साक्षी-रूप असंग रहते हैं। व्यक्ति में जाग्रति, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं में आत्मा साक्षी रहता है। व्यक्ति की जाग्रत अवस्था में भी शरीर के सभी अंग-प्रत्यंग अपने लिए किसी भी प्रकार की आशा न रखते हुए कर्म करते रहते हैं। उदाहरणार्थ पेट भोजन पचाता है, नेत्र वस्तुओं को देखते हैं, पैर चलते हैं, हाथ पकड़ते हैं; पर ये सारी क्रियाएँ किसी अंग-विशेष के लिए नहीं, अपितु सारे शरीर की सहायता के लिए होती हैं। इस प्रकार त्याग की भावना प्रत्येक स्तर पर एक स्वाभाविक अवस्था है। शरीर के सभी अंग अन्तरस्थ चेतना के लिए कार्य करते हैं।
भगवान् कहते हैं कि जो कोई इस प्रकार जाग्रत रह कर कर्म करते हुए जीवन बिताता है, वह सभी कर्मों का सच्चा कर्ता है और मनुष्यों में ज्ञानी होता है। वह किसी कर्म से बन्धन में नहीं पड़ता।
इस अध्याय में मनुष्य को परम सत्य के विषय में उपस्थित शंकाओं का समाधान सांख्य-शास्त्र द्वारा करने तथा कर्मयोग के सिद्धान्त के अनुसार कर्म करने का उपदेश दिया गया है। अतः यह अध्याय 'ज्ञानयोग', 'अभ्यासयोग' तथा 'ज्ञानकर्मसन्यासयोग' भी कहलाता है।
इस भाँति 'ज्ञानविभागयोग' नामक यह चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है।
पंचम अध्याय
कर्मसंन्यासयोग
अर्जुन श्रीकृष्ण से पूछते हैं कि कर्म-संन्यास (सांख्ययोग) और कर्म-सम्पादन 'कर्मयोग', इन दोनों में मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि कर्म-संन्यास तथा निष्काम कर्म, ये दोनों परमानन्द प्रदान करने वाले हैं। वे यह भी कहते हैं कि कर्मयोगी का आचरण अधिक सरल है। कर्मयोगी की भावना सदा त्यागमय होती है, क्योंकि वह अपना कर्तव्य असंग भाव से करता है। केवल अज्ञानी ही यह मानता है कि कर्मयोग और सांख्ययोग ये दोनों भिन्न हैं।
वास्तव में दोनों परस्पर अविच्छेद्य हैं। वे दोनों एक ही फल देने वाले होते हैं। कर्मयोगी की प्रशंसा करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी असंग भाव के कारण कमल-पत्र पर रहने वाले जल-बिन्दु के समान संसार में बन्धन-मुक्त हो कर जीवन-यापन करता है। सांख्ययोगी आत्मानन्द में स्थित हो कर कर्म-संन्यासी बन जाता है और देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूँघना आदि कर्म उसके द्वारा होते हुए भी उन्हें अपने कर्म नहीं मानता। अपितु शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन तथा बुद्धि द्वारा ही ये सब कार्य हो रहे हैं और वह केवल इनका साक्षी मात्र है, ऐसा मानता है।
सांख्ययोग का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि जीव पुरुष और प्रकृति का संयोग है। पुरुष (परमात्मा) न कभी कर्म करता है और न कभी किसी पर कर्म करने के लिए दबाव ही डालता है। सब-कुछ प्रकृति ही करती है। यह पुरुष (ज्ञान) सत्त्व, रज और तम, इन गुणों द्वारा प्रकृति से आवृत होता है। मनुष्य जब अपने को प्रकृति अर्थात् शरीर, मन और बुद्धि मान लेता है, तब वह बन्धन में पड़ जाता है और सतत ध्यान द्वारा जब उसे स्वयं पुरुष अर्थात् परमात्मा होने का भान होता है, तब वह बन्धन-मुक्त हो जाता है; उसकी बुद्धि ब्रह्म में लीन हो जाती है और वह अपने को ब्रह्म समझने लगता है। जब बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो जाती है, तब उसके गौण शरीर, मन और इन्द्रियाँ प्रकृति के जगत् में बाहर सभी को ब्रह्म-रूप ही देखती हैं। तब उसे कुत्ता, मनुष्य, हाथी, वृक्ष आदि सभी दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं में ब्रह्म ही भासित होता है।
कोई व्यक्ति जब शुभ विचारों में संस्थित रहता है, तब उसे सर्वत्र शुभ ही दिखायी देता है और वह दूसरों के प्रति भलाई का व्यवहार किया करता है। वह लांछन-मुक्त होता है और उसके लिए भले-बुरे का भेद समाप्त हो जाता है। जिसे सत्य का ज्ञान होता है, उसमें राग-द्वेष नहीं होता है। वह ब्रह्ममय बन जाता है। अपने स्वय के व्यवहार-सहित प्रकृति के सभी कार्यों का वह साक्षी मात्र रहता है। उसका मन सदा आत्माभिमुख होता है और वह सदा शाश्वत आनन्द का अनुभव किया करता है। ज्ञानी पुरुष जो यह जानता है कभी भी इन्द्रिय-सुख का उपभोग नहीं करता; क्योंकि उसका आदि और अन्त होता है। अन्ततः उसका परिणाम दुःख ही होता है। जो व्यक्ति इच्छा से समुद्भूत काम और क्रोध को अपने वश में रखता है तथा रजोगुण से सत्त्वगुण में ऊर्ध्वगमन करता हुआ, धीरे-धीरे मन को रिक्त कर लेता है, वह योगी कहलाता है। आत्मा के साथ अनुसन्धान कर ऐसा योगी शरीर-त्याग से पूर्व ही जीवन्मुक्त सन्त बन जाता है। जो योगी अन्तरात्मा के आनन्द में मग्न रहता है, वह ब्रह्म के साथ ऐक्य स्थापित कर शाश्वत शान्ति-प्रदायक ब्रह्म को प्राप्त होता है।
शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर के साक्षात्कार से- जो जगत् का कारण-रूप तथा स्वयं जगत्-स्वरूप ही है-हृदय में अज्ञान की ग्रन्थि शिथिल पड़ जाती है और सारी शंकाओं का निवारण हो जाता है। कर्मयोग और सांख्ययोग का विवरण देने के पश्चात् श्रीकृष्ण अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि ये दोनों योग ईश्वर के साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। अब वे बतलाते हैं कि कर्मयोग और साख्ययोग- इन दोनों का सहायक ध्यान-मार्ग अर्थात् ध्यानयोग है। ध्यानयोग में भृकुटियों के मध्य भाग पर विचार केन्द्रित करना पड़ता है। श्वासोच्छ्वास को नियमित करना होता है। इसके बाद मन स्थिर और एकाग्र बन जाता है। एकाग्र मन द्वारा मनुष्य ईश्वर का सतत अनुसन्धान कर सकता है। इस प्रकार कर्मयोग के आचरण से, ध्यान और प्राणायाम द्वारा मन के निग्रह से तथा यह जान कर कि अन्ततः ईश्वर सभी यज्ञों एवं तपों का भोक्ता है, मरण-धर्मा मानव अमर बनता है और परम शान्ति को प्राप्त होता है। अगले अध्याय में श्रीकृष्ण ध्यानयोग का विस्तृत विवरण देते हैं। जो कोई कर्मयोग का आचरण करता है, उसके द्वारा साख्ययोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि अन्य आवश्यक योगों का आचरण भी सहज हो जाता है। ये भिन्न-भिन्न योग परस्पर अभेद्य तथा सहायक होते हैं और व्यक्ति को ईश्वर-साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं।
इस अध्याय में बतलाया गया है कि त्याग अर्थात् निरासक्त वृत्ति समस्त योगों का मूल सिद्धान्त है। त्याग में सभी जीव अनन्त सुख का अनुभव करते हैं। सुषुप्ति में जब मनुष्य सब वस्तुओं से सर्वथा अलिप्त एवं निर्विचार रहता है, तब वह अमोघ सुख का अनुभव करता है। उस अवस्था में बुद्धि, मन और सभी इन्द्रियाँ अपना व्यापार बन्द कर देती हैं और अनजाने ही आत्मा के निकट पहुँच जाती हैं। उस दशा में राजा, रंक तथा सभी प्राणी सहज भाव से सारे भेदभावों को भूल कर तथा अपने कृत्रिम व्यक्तित्व को त्याग कर एक चैतन्य में विलीन हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब जागरूक रह कर इन्द्रिय, मन और बुद्धि की क्रियाओं को त्याग देता है, तब वह परमानन्द-रूप चैतन्य के अपने मूल-स्वरूप में लीन हो जाता है। इस प्रकार त्याग अर्थात् जीव-भाव का अभाव परम पूर्णता का साधन बन जाता है। त्याग के ज्ञान की यह भव्यता और दिव्यता है। व्यक्तित्व के अभिमान से मुक्त हो कर कर्म करने से व्यक्ति समष्टि के साथ एकाकार हो जाता है।
इस प्रकार यहाँ 'कर्मसंन्यासयोग' नामक पंचम अध्याय समाप्त होता है।
षष्ठ अध्याय
ध्यानयोग
इस अध्याय में योगी और संन्यासी दोनों कैसे समान हैं, अर्जुन की इस शंका का भगवान् समाधान करते हैं। भगवान् कहते हैं कि योगी अथवा संन्यासी होने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्य का भली-भाँति पालन करना चाहिए। फल की आशा छोड़ कर अपने कर्तव्य का पालन करने वाला योगी बन जाता है और संसार-सम्बन्धी विचारों को त्याग कर ईश्वर के अविरत स्मरण, शास्त्र के अभ्यास, जप, कीर्तन और ध्यान से व्यक्ति संन्यासी बन जाता है। इस प्रक्रिया से मन और हृदय पवित्र बन जाते हैं। जब व्यक्ति उच्चतर आत्मा के प्रभाव में निम्न जीवात्मा पर नियन्त्रण पाता है, तब मन, इन्द्रियाँ और शरीर पर आधिपत्य हो जाता है। तब आत्मा व्यक्ति का मित्र बन जाता है और जब ऐसा नहीं होता, तो आत्मा ही उसका वैरी बन जाता है। अपने शरीर, मन और इन्द्रियों पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति सुख-दुख में, सर्दी-गरमी में एवं मान-अपमान में शान्त रह सकता है। ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र या वैरी नहीं होता और वह स्वर्ण तथा पाषाण में कोई अन्तर नहीं देखता। पूर्णता प्राप्त योगी अथवा सन्त की यह भूमिका (स्थिति) होती है। वह सब पदार्थों में परमात्मा को देखता है। आत्म-निग्रही और सब इच्छाओं से मुक्त योगी हमेशा अपने मन को ध्यान में निमग्न रखता है।
ध्यानयोग की पूर्वापेक्षाओं का वर्णन करने के पश्चात् श्रीकृष्ण अर्जुन को योग के आचरण की रीति समझाते हैं। कुशा, मृगचर्म और वस्त्र को एक पर एक बिछा कर एकान्त स्वच्छ स्थान में अपना आसन बनायें, फिर सुकर आसन में बैठ कर शरीर, मस्तक और ग्रीवा को सीधा रखते हुए दोनों भृकुटियों के मध्य में ध्यान लगा कर मन एकाग्र करें। आत्म-शुद्धि के लिए इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखते हुए ध्यान और विचार करना चाहिए। निर्भय हो कर गम्भीर मन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दोनों भृकुटियों के बीच ध्यान के केन्द्र पर भगवान् के स्वरूप की उपस्थिति का चिन्तन करें। इस प्रकार जो भगवान् की उपस्थिति का सतत ध्यान करता है, वह परम शान्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
भगवान् श्रीकृष्ण योगाभ्यास के लिए आचार संहिता बतलाते हैं। साधकों को दैनिक व्यवहार में सात्त्विक आहार, सोने तथा जागने का निश्चित समय, यौगिक प्राणायाम, योगासन, सत्संग और स्वाध्याय आदि का नित्य सेवन कर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उसे वायु-रहित स्थान में प्रतिष्ठित दीपक के समान निश्चल और अकम्प रह कर मन को ईश्वर में स्थिर करना चाहिए। जब मन ध्यान द्वारा नियन्त्रित हो जाता है, तब वह अन्तरात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। साक्षात्कार के रसास्वाद का अनुभव होने पर उसे प्रतीत होता है कि तीनों लोकों में पाने वाली वस्तु अन्य कुछ भी नहीं है। उस अवस्था में संसार का भीषण-से-भीषण दुःख भी उसे चलायमान नहीं कर सकता। योग के अभ्यास द्वारा इस प्रकार का आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। यह जान कर व्यक्ति को आजीवन दृढ़तापूर्वक एवं हृदय की दुर्बलता को दूर कर योग-साधना करनी चाहिए। साधना आजीवन करने योग्य प्रक्रिया है। प्रतिपल, हर घड़ी ईश्वर-चिन्तन चलता रहना चाहिए। पूर्व-संस्कार एवं स्वभाव के कारण मन जब-जब ध्यान से विषयों की ओर चलायमान होने लगे, तब-तब प्रयासपूर्वक उसे ध्यान पर खींचना चाहिए। ध्यान के इस प्रकार के सतत आचरण से ध्यान, ध्यानी और ध्येय एकाकार हो जाते हैं और तब वह व्यक्ति परमानन्द का अनुभव करता है। ऐसा निग्रही मन वाला योगी आत्मा को सब जीवों में और सब जीवों को आत्मा में देखने लगता है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'सबमें मुझे और सबको मुझमें देखने वाला व्यक्ति मुझसे अलग नहीं रह सकता और न मैं ही उससे अलग हो सकता हूँ। ऐसा योगी अथवा जीवन्मुक्त पुरुष ईश्वर के हाथ का एक साधन मात्र बन कर रहता है।
समदृष्टि और मन के सन्तुलन का गुणगान करने वाली श्रीकृष्ण की वाणी सुन कर अर्जुन कहते हैं कि 'मन चंचल, प्रमथन करने वाला, दृढ़ और बलवान् है। वायु के समान उसे वश में करना कठिन है।' अतः अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि योग साधना में जो व्यक्ति सफल नहीं होता है, उसकी क्या गति होती है। क्या ईश्वर-साक्षात्कार एवं स्वर्गीय आनन्द-इन दोनों से वह वंचित रहता है? श्रीकृष्ण कहते हैं कि वैराग्य और अभ्यास से मन को वश में रखा जा सकता है। योग-भ्रष्ट साधक पवित्र एवं समृद्ध व्यक्ति के अथवा योगियों के कुल में जन्म लेता है और मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुन प्रयत्नशील होता है। श्रीकृष्ण यह भी कहते हैं कि जो उनके भक्त हैं, वे योगियों में श्रेष्ठ हैं। अतः वे ऐसा योगी बनने का अनुरोध करते हैं कि जो तपस्वियों, शास्त्रज्ञों और याज्ञिकों से भी श्रेष्ठ होता है।
इस अध्याय में श्रीकृष्ण भगवान् यह शिक्षा देते हैं कि मानव जाति के उद्विकास के प्रत्येक प्रकार और प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान ईश्वर-चैतन्य प्राप्त करने का साधन है। वे यह भी कहते हैं कि ईश्वर-चैतन्य की प्राप्ति सभी योगों का ध्येय है। प्रत्येक योग में अर्थात आध्यात्मिक साधना की प्रत्येक विधि में मन का ही प्रमुख भाग रहता है। मन को जब पूर्ण समझ-बूझ के साथ ईश्वर की ओर मोड़ा जाता है, तब मनुष्य का जगत् के प्रति दृष्टिकोण, उसकी मनोवृत्ति और इच्छाएँ स्वत बदल जाती हैं। निराहारी की इन्द्रियाँ विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, पर उसकी विषय-लालसा बनी रहती है। परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर यह लालसा भी निवृत्त हो जाती है। इस भाँति सतत ध्यान से ईश्वर-चैतन्य का अनुभव होने पर विषमता में एकता दिखायी देने लगती है और सभी इच्छाओं का अन्त हो जाता है।
इस प्रकार यह 'ध्यानयोग' नामक छठवाँ अध्याय समाप्त होता है।
सप्तम अध्याय
ज्ञानविज्ञानयोग
पिछले अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन को भक्तयोगी बनने को कहते हैं जो कि अन्य सबसे श्रेष्ठ है। श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अब उन्हें भगवद्-ज्ञान का रहस्य बतलायेंगे जिससे कि व्यक्ति भगवान् के विभूति-बल-ऐश्वर्य-सहित पूर्ण ज्ञान से भक्ति की विविध प्रणालियों का आचरण तथा अपने मन को भगवान् में निरन्तर स्थापित कर सके। इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात् अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि सहस्रों मनुष्यों में कोई एक ही पूर्णत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और ऐसे प्रयत्नशील व्यक्तियों में कोई एक ही व्यक्ति मुझे यथार्थतः जान पाता है।
भगवान् प्रथम अपरा (निम्न कोटि की) और परा (उच्च कोटि की) प्रकृति का वर्णन करते हैं। अपरा प्रकृति आठ प्रकार की है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। परा प्रकृति जीवन-तत्त्व है जिसके कारण समस्त संसार टिका हुआ है। सभी प्राणी इन दो प्रकृतियों से उत्पन्न हुए हैं और उनके सर्जन, रक्षण तथा विनाश का ईश्वर कारण है।
श्रीकृष्ण कहते हैं कि स्वयं ईश्वर ही समस्त सृष्टि का एकमात्र कारण और परम आधार है। समग्र ब्रह्माण्ड भगवान् की अभिव्यक्ति है तथा भगवान् द्वारा व्याप्त है। धागे में पिरोयी हुई मणियों के समूह के समान विश्व ईश्वर में पिरोया हुआ है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं-"जल में रस, सूर्य और चन्द्र में तेज, सम्पूर्ण वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पौरुष मैं ही हूँ।" वे बतलाते हैं कि जगत् के दृश्य तथा अदृश्य सभी पदार्थों में उनका निवास है और समस्त जगत् का आदि कारण वे ही हैं। माया की आवरण-शक्ति के कारण जगत् उनकी उपस्थिति जानने में असमर्थ रहता है। एकमात्र भगवान् का आश्रय लेने वाला ही इस दिव्य माया से पार हो सकता है। सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुणों एवं द्वन्द्वों से मोहित होने के कारण भगवान् मनुष्य को दिखायी नहीं देते। सांसारिक मनुष्य की बुद्धि पर माया का आवरण चढ़ा रहता है। प्रकृति के तीनों गुण जब एकत्र हो जाते हैं, तब माया का आवरण होता है। माया के कारण जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य भगवद्-भक्ति करना भूल जाते हैं। वे मानते हैं कि यह जगत् और दृष्य पदार्थ ही सत्य हैं। वे असुरों जैसा व्यवहार करते हैं और जन्म-मरण के चक्र में घूमते हुए दुख में डूबे रहते हैं।
आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी-ऐसे चार प्रकार के गुणवान् व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करते हैं। इसमें एकाग्र मन से भक्ति करने वाले ज्ञानी मनुष्य भगवान् को अधिक प्रिय हैं। अनेक जन्म-मृत्यु और दुःखों के पश्चात् मनुष्य को यह प्रतीत होता है कि शाश्वत श्रीकृष्ण भगवान् अर्थात् परमात्मा ही सत्य हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में दुर्लभ हैं।
जिनकी बुद्धि अनेक इच्छाओं, वासनाओं से प्रेरित है, ऐसे लोग अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवी-देवताओं की उपासना करते हैं और शास्त्रोक्त विधियों को अपनाते हैं। वास्तव में सभी देवी-देवता एक ही परमात्मा के विविध रूप हैं। व्यक्ति अपने स्वभाव, श्रद्धा और जीवन के आदर्श के अनुसार अपनी भक्ति का फल प्राप्त करते हैं। ऐसे अल्प ज्ञानी लोगों द्वारा प्राप्त परिणाम (फल) सीमित, सान्त होता है; क्योंकि वे ईश्वर की सर्व-व्यापकता को भूल कर अपने सीमित ज्ञान से ही विशिष्ट देवता की उपासना करते हैं। देवता अथवा इष्टदेव तो मन को एकाग्र करने का एक साधन मात्र है। उसे ही साध्य नहीं मान बैठना चाहिए। मनुष्य को एकाग्र मन से इष्ट-वस्तु का अविरत ध्यान करना चाहिए। इससे धीरे-धीरे विचारों का विराम हो कर वह परमात्मा का, सर्वव्यापक चैतन्य का अनुभव कर सकेगा। इस चैतन्य भाव में सभी प्रकार के नाम, रूप तथा व्यक्तित्व का विलय हो जाता है और केवल सद्वस्तु की सत्ता शेष रहती है। जीव का अज्ञान दूर करने के लिए, मानव को देवता, नर को नारायण बनाने के लिए और जीवात्मा को अपनी मूल-प्रकृति अर्थात् पूर्णता प्राप्त कराने के लिए भगवान् अनेक नाम-रूपों से जगत् में प्रकट होते हैं।
भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों के विषय में जानते हैं; पर उन्हें कोई भी नहीं जानता। राग-द्वेष, सुख-दुख, गरमी-सर्दी, आनन्द-विषाद, हर्ष-शोक, जय-पराजय, मान-अपमान आदि इच्छाओं और घृणा से उत्पन्न द्वन्द्वों के कारण सभी जीव माया में फँसे हुए हैं। वे ईश्वर के सर्वव्यापी अस्तित्व को भूल कर जन्म-मरण के दुःखों को भोगते रहते हैं। जो ईश्वर को सम्पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, वह ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञादि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अगले अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण इनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे।
जो मनुष्य अपने जीवन-भर भगवान् का स्मरण नहीं करता, वह अपने मृत्यु-समय में भी भगवान् का नाम-स्मरण नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति केवल मृत्यु-समय में भी भगवान् के नाम का जप अथवा उनके दिव्य स्वरूप का चिन्तन करता है तो सर्वोच्च अविनाशी, परमात्म-स्वरूप को प्राप्त हो जाता है; परन्तु जो मनुष्य जीवन-भर ईश्वर का नाम नहीं लेता, वह मृत्यु के समय उनका स्मरण कर सकेगा, यह कठिन है।
इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणों के कार्य में ईश्वर कारणीभूत है। अज्ञान के कारण मनुष्य मोहान्ध बन जाता है और अपने-आपको इन तीनों गुणों का परिणाम-मन, इन्द्रिय और शरीर मानता है। समस्त संसार तीनों गुणों के अन्योन्य व्यवहार पर टिका हुआ और संचालित है। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक-शक्ति प्रदान की है जिसके द्वारा वह तीनों गुणों से परे हो कर उनके कारण-रूप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है।
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के किसी भी परिणाम अर्थात् मन, इन्द्रियों और शरीर के साथ अपना तादात्म्य न मान कर भक्ति द्वारा व्यक्ति ईश्वर के साब सायुज्य-मुक्ति प्राप्त कर सकता है। माला की मणियों के आधार-धागे के रूप में परम चेतन-तत्त्व जगत् में कार्य कर रहा है, इस बात का साधक को सतत ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति के सभी अंग एक ही चेतना द्वारा संचालित तथा परस्पर सम्बद्ध हैं। इसी प्रकार समस्त विश्व सर्वव्यापी ईश्वर के चैतन्य के कारण टिका हुआ है। भगवान् कहते हैं कि महत्तम चेतना की उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार किसी भी साधन द्वारा कर सकता है और ईश्वर में विलीन हो कर परमानन्द की प्राप्ति कर सकता है। जो यह जानते हैं कि जन्म-मृत्यु, वृद्धावस्था और अनेक व्याधियों से दुःख उत्पन्न होते हैं, यह भी अनुभव करते हैं कि सर्वोच्च ध्येय तथा मानव की सभी प्रवृत्तियों का पर्यवसान केवल ईश्वर ही है, और श्रद्धा तथा ज्ञानपूर्वक आचरण करते हैं, वे उस परम तत्त्व को पा लेते हैं और फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता।
इस प्रकार यह 'ज्ञानविज्ञानयोग' नामक सप्तम अध्याय समाप्त होता है।
अष्टम अध्याय
अक्षरब्रह्मयोग
परमात्मा के सभी दिव्य रूपों की विविधताओं को जानने की इच्छा से अर्जुन ने पिछले अध्याय में बतायी गयी तत्त्वज्ञान की पारिभाषिक व्याख्याओं पर प्रकाश डालने की श्रीकृष्ण भगवान् से प्रार्थना की है। उन्होंने सात प्रश्न पूछे हैं "ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञ क्या हैं और मृत्यु के समय समाहित-चित्त पुरुष आपको किस प्रकार जान सकता है?"
श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं कि परम और अविनाशी तत्त्व को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म अक्षर, अविकारी, सर्वव्यापक, स्वयंभू, स्वयंप्रकाश और सभी घटनाओं का परम कारण है। उस ब्रह्म का प्रत्यगात्मभाव अथवा जीव-चैतन्य अध्यात्म कहलाता है। देश, काल, नाम और रूप से बाधित परम चैतन्य ही अध्यात्म है। जगत् की जीव-सृष्टि तथा जीवात्मा का अस्तित्व, व्यक्तता एवं स्थिति की कारणभूत शक्ति को कर्म कहते हैं। जिस शक्ति के कारण ईश्वर एक से अनेक रूप धारण करता है, वही यह शक्ति है। सभी क्षर वस्तुएँ अर्थात् सृष्टि के पाँच तत्त्वों से बनी हुई सभी वस्तुएँ, आदि और अन्त वाले सभी पदार्थ, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ और शरीर अधिभूत कहलाते हैं। विश्वात्मा अथवा दिव्य प्रज्ञा देव-रूप है, जो उसके अंश हैं। ईश्वर सबका नियामक, स्वामी और जन्मदाता है। वह आदि-पुरुष एवं सूत्रात्मा है। समस्त विश्व के प्रत्येक चर और अचर पदार्थों की प्राण-शक्ति वही है। इसी से वह अधिदैव कहलाता है। सभी यज्ञों का अधिष्ठाता देव एवं शरीर में अन्तर्यामी रूप से स्थित शरीर का चैतन्य साक्षी होने के कारण वह अधियज्ञ कहलाता है।
अर्जुन के अन्तिम प्रश्न का समाधान करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करने वाला ईश्वर को ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य का आगामी जन्म उसके मृत्यु के समय के अन्तिम विचारों के अनुसार होता है। जीव मृत्यु-समय में जिस वस्तु का विचार करता है, वही वस्तु उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। भूतकाल के अर्थात् पूर्व-जन्म के अपने विचारों एवं इच्छाओं के अनुसार ही हमारा वर्तमान जन्म और जीवन प्राप्त हुआ है और अब वर्तमान जीवन में दृढ हुए विचारों के अनुसार ही अगला जन्म निश्चित होगा। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु समय मन और प्राण-सहित वासना-जो सूक्ष्म देह या जीव कहलाता है-भौतिक शरीर को त्यागते हैं।
जीव का स्थूल शरीर से वियोग ही मृत्यु है। इस शरीर को अस्तित्व में लाने वाला संवेग बन्द होता है, तब मृत्यु होती है; परन्तु ऐसा कब होगा, यह कोई नहीं जानता और इसीलिए मृत्यु के अन्तिम क्षण की किसी को खबर नहीं होती।
इसीलिए भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने पर ही वह अन्तिम समय में ईश्वर का स्मरण कर सकेगा। 'जब मन और बुद्धि मुझमें लीन होगी, तब तुम निस्सन्देह मुझे प्राप्त कर सकोगे।' भगवान् श्रीकृष्ण प्रतिक्षण योगाभ्यास की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति मन को ईश्वर में स्थित कर आजीवन ध्यान करता है तो अन्त समय में भी ईश्वर-चैतन्य अथवा ईश-विचार उसमें अवश्य स्थित रहेगा और वह सांसारिक विषयों में कभी आसक्त नहीं होगा। अतः हर व्यक्ति को द्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सूर्य, चन्द्र और ताराओं के प्रकाश का उद्गम स्थान एवं अज्ञानान्धकार को दूर करने वाले परब्रह्म परमात्मा का हमेशा ध्यान करना चाहिए।
सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, प्राणिक एवं मानसिक स्तरों पर व्यक्तित्व में सामंजस्य न होने के कारण अपने अस्तित्व के आधार को भूल जाता है और दुःखी होता है। जैसे सरोवर के विक्षुब्ध जल के कारण उसके तल में पड़े हुए कंकड़ दिखायी नहीं देते और जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब भी नहीं दिखायी देता, वैसे ही इस विसवादिता के कारण आत्मा में उसके अन्तर्गत व्यक्तित्व का भान नहीं होता। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को एक ऐसी युक्ति बतलाते हैं जिसके अभ्यास से व्यक्ति अपने में आवश्यक सुसंगतता ला कर ईश-चैतन्य पा सकता है।
श्रीकृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को दोनों भृकुटियों के मध्य में मन को एकाग्र कर ॐ के जप के साथ प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के लिए मेरुदण्ड और गरदन को सीधा रख कर सुखपूर्वक आसन पर बैठना चाहिए। ऐसा करने से शारीरिक अंगों में सुसंगतता प्राप्त होती है और शरीर के सभी अंगों में प्राण का नियमित संचार होता है। जाग्रत अवस्था में मन का स्थान आज्ञाचक्र अर्थात् दोनों भृकुटियों के बीच का स्थान है। व्यक्ति जब इस स्थान पर ध्यान केन्द्रित करता है, तब इन्द्रियाँ और मन शान्त हो जाते हैं। 'ॐ' के जप से नाड़ी-तन्त्र में सुमेल हो जाता है और साधक का समग्र व्यक्तित्व एक ही चैतन्य का अनुभव करने लगता है और धीर-धीरे उसे परम चैतन्य का साक्षात्कार होने लगता है। ऐसा योगी जो योगाभ्यास द्वारा इन्द्रिय-निग्रह करता है, प्राणायाम करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, मृत्यु-समय में भी ब्रह्म के वाचक अथवा प्रतीक 'ॐ' का जप करता रहता है। वह परम श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से उसे पुनः इस मर्त्यलोक में लौट कर नहीं आना पड़ता। इसका भावार्थ यह है कि ध्यान के नित्य अभ्यास द्वारा व्यक्ति को ईश-चैतन्य में सदा संस्थित रहना चाहिए। ऐसा होने पर ही मृत्यु-समय में दिव्य चैतन्य को प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा। मर्त्यलोक दुःख का स्थान और अनित्य अर्थात् विनाशशील है। ईश-चैतन्य प्राप्त करने वाले परम गति (मोक्ष) को प्राप्त कर लेते हैं।
रजोगुण-प्रधान विश्वविधाता ब्रह्मा कहलाते हैं। सत्त्वगुण-प्रधान विश्व का धारण और पोषण करने वाले विष्णु और तमोगुण-प्रधान विश्वसंहारक रुद्र अर्थात् शंकर कहलाते हैं। ८,६४,००,००,००० मानवीय वर्ष से ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे सौ वर्ष का ब्रह्मा का जीवन है। यज्ञ और सत्कर्मों से व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुँचता है; पर वह भी देश, काल और कर्तृत्व के बन्धन से प्रतिबन्धित है। दीर्घ काल तक सत्कर्मों का फल भोगने के पश्चात् जीव पुनः इस संसार में जन्म लेता है।
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं "जो मनस्वी एक हजार युग से बना हुआ ब्रह्मा का एक दिन और एक हजार युग की उनकी एक रात्रि को जानते हैं, वे रात और दिन का रहस्य समझते हैं। दिन निकलते ही विश्व की सभी वस्तुएँ अव्यक्त से व्यक्त में प्रकट होती हैं और रात होते ही अर्थात् प्रलय के समय वे सब पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के दिन और रात के बीच अनन्त जीव जन्म लेते और मरते हैं, पर केवल ईश्वर ही इन सबका शाश्वत साक्षी-रूप एवं अलिप्त रहता है। अतः जो व्यक्ति मृत्यु-समय में परमात्मा को शाश्वत साक्षी-रूप में स्मरण करता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता और देश, काल तथा कारण से परे परम तत्त्व में विलीन हो जाता है।"
मृत्यु-समय में योगी जन ईश्वर की अनुभूति किस प्रकार करते हैं, इसके विषय में श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। ईश्वर-साक्षात्कार के बिना कोई भी व्यक्ति जन्म-मरण के चक्र से नहीं छूट सकता। ब्रह्मा के लोक तक पहुँच कर भी वह जन्म-मरण के फेरे नहीं टाल सकता। अतः योग-साधना करने वाले साधक जिन दो मार्गों से मरणोपरान्त प्रयाण करते हैं और वापस लौटते हैं, उनके सम्बन्ध में श्रीकृष्ण विवेचन करते हैं।
जब अग्नि, तेज और दिवस के अभिमानी देवताओं का आधिपत्य होता है, जब शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य का छह मास का उत्तरायण काल होता है, उस समय शरीर त्यागने वाले योगी प्रथम ब्रह्मलोक में जाते हैं और पश्चात् परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः संसार में वापस नहीं आते। इसे 'क्रम-मुक्ति' अथवा 'उत्तर-मार्ग' या 'देवयान' कहा जाता है। जो अज्ञानी, सांसारिक विषयों में आसक्त, फलाशा से यज्ञ करने वाले जब धून एवं रात्रि के अभिमानी देवताओं का आधिपत्य होता है, कृष्ण पक्ष होता है तथा जो जब सूर्य की गति छह मास के लिए दक्षिण की ओर (दक्षिणायन) होती है तब मरते हैं, वे चन्द्रलोक को (पितरों के स्वर्ग को) प्राप्त होते हैं। वे अपने सत्कर्मों का फल भोगने के पश्चात् पुनः इस लोक में वापस लौटते हैं। इसे प्रकाश-हीन मार्ग अर्थात् 'दक्षिण-मार्ग' या 'पितृयान' कहते हैं।
श्रीकृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि योग-मार्ग पर चलने वाले मुमुक्षु इन दो मार्गों को जानते हैं और इसलिए फल की आशा से कभी यज्ञ, शास्त्राध्ययन या दान आदि नहीं करते; क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त सभी कुछ दुःखदायी और क्षणिक है। अतएव वे हमेशा ईश-चैतन्य तथा ईश्वरानुसन्धान में ही डूबे रहते हैं और अन्त में सर्वोत्कृष्ट कारण-रूप परम पद को प्राप्त करते हैं।
इस अध्याय में श्रीकृष्ण मानव जीवन के महत्त्व का वर्णन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि चौरासी लाख मानवेतर योनियों को पार करने के बाद जीव भगवद्-कृपा से मनुष्य-जन्म पाता है। अतः श्रीकृष्ण चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इस मानव-जन्म में यदि व्यक्ति ईश्वर-प्राप्ति के अलभ्य अवसर का लाभ न ले और मोह, लोभ तथा ईर्ष्या जैसे पाशवी तत्त्वों के बीच अपना सारा जीवन व्यतीत करता रहे तो उसे मृत्यु-समय में ईश्वर का स्मरण नहीं हो सकता। उसे मरणोत्तर पुनः मानवेतर योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अतः भगवान् योग और ध्यान के अभ्यास पर जोर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति मृत्यु-समय में सांसारिक जंजाल का चिन्तन करने के बदले केवल ईश-चिन्तन में ही मग्न रहे।
इस प्रकार 'अक्षरब्रह्मयोग' नामक यह अष्टम अध्याय समाप्त होता है।
नवम अध्याय
राजविद्याराजगुह्ययोग
श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुन को श्रद्धावान्; दोष-दृष्टि-रहित एवं पवित्र दिव्य ज्ञान का पात्र समझ कर उनसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें प्रत्यक्ष फलप्रद राजविद्या (सब विद्याओं का राजा) एवं राजगुह्य (सब गुप्त रखने योग्य भावों का राजा) बतलाऊँगा। वे कहते हैं-"यह विद्या अविनाशी है और इसे जान लेने पर व्यक्ति दुःख-रूप संसार से मुक्त हो जाता है।" भगवान् कहते हैं कि इस ज्ञान में-उसके व्यक्त-अव्यक्त रूप में श्रद्धा के अभाव से लोग ईश्वर-प्राप्ति में असफल होते हैं और संसार में दुःख भोगते हैं।
भगवान् कहते हैं कि यह समस्त जगत् उनसे व्याप्त है और जैसे सदा ही आकाश में स्थित रहने वाली सर्वत्र गमनशील तथा महान् वायु का आकाश से सम्पर्क नहीं होता है वैसे ही ये सब प्राणी उनमें स्थित हैं। वे विश्व के सर्जक, पालक और संहारक होते हुए भी इन सब क्रियाओं से उदासीन तथा असंग रह कर केवल साक्षी-रूप हैं। जिन्हें ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी लोग उनको प्रकृति का स्वरूप मानते हैं और धर्म की रक्षा के लिए जब वे अवतार लेते हैं; तब उन्हें मरण-धर्मा मनुष्य के समान समझते हैं। ऐसे व्यक्ति विश्व में विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर पाते और शरीर में रहने वाले आत्मा के विषय में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वे विश्व की विविधता में एकता नहीं देखते। लहरों के नीचे वाले समुद्र को वे भूल जाते हैं। क्षणभंगुर विषयों के पीछे भागते हुए वे शाश्वत सत्य को चूक जाते हैं। उन्हें सारासार विवेक नहीं होता। कुछ साधक ज्ञान-यज्ञ के द्वारा भगवान् की उपासना करते हैं। कुछ सत्य के ज्ञाता ज्ञानी जन परमार्थ-दर्शन-रूप अभेद भावना से उपासना करते हैं। कितने ही साधक पृथक् भावना से उपासना करते हैं, कितने ही साधक निराकार ईश्वर को सर्वरूप परमेश्वर के रूप की अनेक प्रकार से उपासना करते हैं तथा कितने ही साधक सर्वदा कीर्तन करते हुए भगवान् को भजते हैं।
श्रीकृष्ण भगवान् अपने सर्वात्म-भाव का दिग्दर्शन कराते हैं। वे कहते हैं कि वे इस जगत् के माता-पिता तथा पितामह हैं। वे ही कर्म-फल का विधान करने वाले हैं। जानने योग्य तत्त्व ओंकार तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। वे ही औषधि तथा सब प्रकार की वनस्पति हैं। वे ही पुजारी और पूज्य दोनों हैं। वे सूर्य में से उष्णता को बिखेर कर वर्षा करते हैं। वे ही सत् तथा असत्, अमरत्व और मृत्यु सब-कुछ हैं। सूर्य, चन्द्र और अग्नि के समान देवता उनके शरीर के ही अंग हैं। वे कहते हैं कि वे ही हवन हैं और वे ही हवन-सामग्री हैं। पुण्य-संचय के कारण गुणी जन भगवान् के व्यक्त-स्वरूप को भजते हैं। ऐसे भक्त स्वर्ग में सुखों का उपभोग करने के बाद पुण्य-क्षय होने पर पुनः मर्त्यलोक में लौट कर आते हैं।
जो भक्त गण अन्य कोई कामना न रखते हुए भगवान् का ही अनन्य भाव से नित्य स्मरण करते तथा उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भगवान् पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं और उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अज्ञान के कारण जो लोग अन्य देवी-देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी उनकी ही पूजा करते हैं। वे नहीं जानते कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। इसलिए ऐसे कामना वाले भक्त स्वर्ग-सुख पाने के बाद पुन मृत्युलोक में वापस आते हैं। जो भक्त निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। भक्त को तो केवल भक्ति ही प्यारी होती है। वह अन्य किसी वस्तु या सम्पदा की इच्छा नहीं करता। जो भक्त भगवान् को पत्र, पुष्प, फल और जल मात्र भी भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, वे ऐसे भक्त से उसे स्वीकार कर लेते हैं। भक्त द्वारा अर्पण की गयी वस्तु की गुणवत्ता या मूल्य को भगवान् नहीं देखते। वे तो केवल भक्त की भावना और भक्ति को देखते हैं।
अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भक्ति से ईश्वर की उपासना करता है, तो वह भी साधु वृत्ति वाला माना जाता है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। श्रीकृष्णण अर्जुन को यह दृढ़ विश्वास दिलाते हैं कि जो भक्त पूर्ण हृदय से अपनी आत्मा मुझे समर्पित करता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वे कहते हैं कि खाना, पीना, पढ़ना, तप करना, दान करना आदि जो भी कर्म तुम दैनिक जीवन में करो, वह नि स्वार्थ भाव से मुझे अर्पण करो। निकृष्ट जन्म वाला मनुष्य भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। केवल राजर्षि, ब्राह्मण आदि ही नहीं अपितु स्त्रियाँ, वैश्य तथा शूद्र भी मेरे परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे अर्जुन ! मुझमें अपने मन को स्थिर कर, मेरा भक्त बन, मेरे लिए ही यज्ञ कर, मुझे ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे में एकीभाव करके मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा।
इस अध्याय में भगवान् प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पण भावना से करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार किया गया प्रत्येक कार्य भक्ति का प्रतीक बन जाता है और ईश्वर का सतत स्मरण रखने में सहायक होता है। भगवान् को किसी सांसारिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं कि उन्हीं में सारा जगत् समाया हुआ है, परन्तु वे स्वयं उसमें स्थित नहीं हैं। लहरें समुद्र में हैं; परन्तु समुद्र लहरों में समाया हुआ नहीं है। इस अध्याय में भगवान् एक गुप्त बात प्रकट करते हैं। उनसे पृथक् किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे ही विश्व में व्यक्त और अव्यक्त सत्य हैं। जीवन की प्रत्येक अवस्था में और स्थिति में इस सत्य एवं अस्तित्व के रहस्य का जिन्हें भान है, वे निश्चय ही ईश्वर को प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार 'राजविद्या' एवं 'राजगुह्ययोग' नामक नवाँ अध्याय समाप्त होता है।
दशम अध्याय
विभूतियोग
परमेश्वर के सबसे गुह्य गुणों, विभूतियों और सत्य स्वरूप के विषय में अर्जुन की जिज्ञासा देख कर भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन के साथ-साथ सम्पूर्ण मानव-जाति के हित और कल्याण के लिए यह गुह्य ज्ञान प्रेमपूर्वक अर्जुन को सुनाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे स्वयं सबके आदि कारण हैं। अतएव देवता और ऋषि गण भी उनकी उत्पत्ति (प्रभव) को नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति यह जानता है कि भगवान् अजन्मा, अनादि एव लोकों के महान् ईश्वर हैं, वह मनुष्यों में मोह-रहित हो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जीवों के विभिन्न भाव यथा बुद्धि, आत्मज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सहनशीलता, सत्य- भाषण, दम, शम, सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भय एवं निर्भयता-ये सब ईश्वर से ही होते हैं। मेरे ही प्रभाव से सम्पन्न सात महर्षि जन, उनसे भी पूर्व के चार सनकादि महर्षि, मनु आदि सब मेरे (भगवान् के) ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और उनसे ही संसार के समस्त प्राणी जन्म प्राप्त किये हैं। जो कोई भगवान् की इन अनेक विभूतियों और योग-शक्तियों को तत्त्व से जानता है, वह निःसन्देह योग में स्थित हो जाता है। भगवान् ही सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति के कारण हैं और उनसे यह समस्त जगत् प्रवर्तित हो रहा है। इस प्रकार जान कर विवेकी जन उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उन्हें आत्म-समर्पण करते हैं, उनका ध्यान धरते हैं और उन्हीं में आनन्द को प्राप्त होते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें प्रेमपूर्वक भजते हैं, उन्हें वे बुद्धियोग प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वे उन्हें (भगवान् को) प्राप्त होते हैं। श्रीकृष्ण यह भी कहते हैं कि उन पर अनुग्रह करने हेतु भगवान् उनके अन्तःकरण में विराज कर अज्ञान-रूपी अन्धकार को प्रकाशमान ज्ञान-रूपी दीपक से नाश करते हैं।
श्रीकृष्ण की इन बातों को सुन कर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि 'नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषियों ने भी यही बात कही है। आपने जो कुछ कहा, उसे मैं सत्य मानता हूँ। देव अथवा दानव आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप स्वयं ही अपने-आपको जानते हैं। आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों का वर्णन करने में समर्थ हैं जिनके द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त कर आप स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार चिन्तन करता हुआ आपको जान सकता हूँ, कृपया यह बतलाइए। किन-किन पदार्थों अथवा भावों में मैं आपका चिन्तन करूँ? हे कृष्ण, अपने ऐश्वर्य तथा विभूतियों को मुझे पुनः सुनाइए। आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है।'
तब भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं - "मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। समस्ज जीवों का आदि, मध्य और अन्त मैं ही हूँ। अदिति के बारह पुत्रों में विष्णु मैं हूँ। ज्योतियों में रश्मियों से युक्त सूर्य मैं हूँ। (सात या उनचास) मरुद्गणों में मरीचि मैं हूँ। नक्षत्रों में चन्द्रमा मैं हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इन्द्र, इन्द्रियों में मन और भूत प्राणियों में चेतना मैं ही हूँ। एकादश रुद्रों में शंकर मैं हूँ। यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुवेर मैं हूँ। आठ वसुओं में अग्नि देवता मैं हूँ। पर्वतों में मेरु मैं हूँ। पुरोहितों में उनका मुख्य पुरोहित बृहस्पति मैं हूँ। सेनानायकों में स्कन्द मैं हूँ और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु मैं हूँ। वाणी में एकाक्षर ओंकार मैं हूँ। यज्ञों में जप-यज्ञ मैं हूँ और स्थावरों में हिमालय मैं हूँ। सभी वृक्षों में पवित्र अश्वत्थ (पीपल) मैं हूँ। देवर्षियों में नारद, गन्धर्वो में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि और अश्वों में उच्चैः श्रवा मैं ही हूँ। शक्तिशाली हाथियों में इन्द्र का हाथी ऐरावत मैं हूँ। मनुष्यों में राजा मैं हूँ। शस्त्रों में बज्र मैं हूँ। गौओं में दिव्य कामधेनु मैं हूँ। सन्तान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ। सर्पों में वासुकि मैं हूँ। नागों में शेषनाग मैं हूँ। जलचरों का राजा वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्थमा मैं हूँ। शासकों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रह्लाद मैं हूँ। गणना करने वालों में काल मैं हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह मैं हूँ। पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु मैं हूँ। शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। मत्स्यों में मगरमच्छ मैं हूँ। नदियों में गंगा मैं हूँ। हे अर्जुन, संक्षेप में समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अन्त मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म-विद्या मैं हूँ। विवाद करने वालों में तत्त्व-निर्णायक बाद मैं हूँ। अक्षरों में अकार मैं हूँ। समासों में द्वन्द्व समास मैं हूँ।" भगवान् कहते हैं- "अक्षय काल मैं हूँ और विराट्र स्वरूप विधाता मैं हूँ। सबका नाश करने वाला मृत्यु मैं हूँ और वैभवशाली का अभ्युदय भी मैं ही हूँ। खी-वाचक गुणों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गेय मन्त्रों में बृहत्साम में हूँ। छन्दों में गायत्री छन्द मैं ही हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ और ऋतुओं में वसन्त ऋतु मैं हूँ। छल-कपट करने वालों में छूत मैं हूँ। तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्त्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव मैं हूँ। पाण्डवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में ब्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। दमन करने वालों में दमन-शक्ति, विजय चाहने बालों में कूटनीति, गोपनीय भावों में मौन तथा तत्त्वज्ञानियों में तत्त्वज्ञान मैं ही हूँ। सब जीवों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। मुझसे रहित किसी चर और अचर का अस्तित्व नहीं है। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अन्त नहीं है। इस सम्पूर्ण जगत् को मैं अपने एक अंश मात्र से धारण किये हुए हूँ।"
इस अध्याय में अर्जुन भगवान् से उनकी विभूतियों, उनकी योग-शक्ति तथा उनके ध्येय स्वरूप को जानना चाहते थे। अतः परम प्रभु उन्हें ध्यान की प्रक्रिया समझाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मन का उद्गम स्थान अर्थात् शुद्ध चेतना प्राप्त करने के लिए ध्यान में मन को चेतना के स्थूल स्तर से सूक्ष्म स्तर की ओर ले जाना चाहिए। मन सदैव बहिर्मुख हुआ करता है और इन्द्रियों की स्पर्शानुभूति पर निर्भर करता है। भगवान् के कथनानुसार जब मनुष्य को यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि केवल भगवान् ही मूल-तत्त्व के रूप से सभी पदार्थों में विद्यमान हैं, तब मन को अनुभूति के स्थूल स्तर पर यह विश्वास होने लगता है कि विषय का हार्द अर्थात् चेतना ही उसका मूल-स्वभाव है। उसके पश्चात् आन्तरिक चेतना को सहज ही अबाध रूप से बाह्य चेतना का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार भगवान् यह शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति भागवतीय चेतना में सदैव स्थित रह सकता है।
इस प्रकार 'विभूतियोग' नामक यह दशम अध्याय समाप्त होता है।
एकादश अध्याय
विश्वरूपदर्शनयोग
गुह्य अध्यात्म-ज्ञान, दिव्य ऐश्वर्य एवं विभूतियों के विषय में भगवान् श्रीकृष्ण का निरूपण सुनने के बाद अर्जुन ने कहा "अब मेरा भ्रम नष्ट हो गया है।" वह दिव्य विश्वरूप देखने की अपनी इच्छा प्रकट करते हुए प्रार्थना करते हैं "हे कृष्ण! यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं आपका दिव्य स्वरूप देखने योग्य हूँ, तो कृपया आप अपने अविनाशी विराट् स्वरूप का दर्शन करायें।" अपने प्रिय एवं श्रद्धालु भक्त की विनती सुन कर श्रीकृष्ण ने कहा : "हे अर्जुन! मेरे अलौकिक नाना विध, नाना वर्ण तथा आकृति-विशिष्ट शत-शत तथा सहस्र-सहस्र रूपों को देखो। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों तथा अनेक आश्चर्यमय मेरे रूपों को जिन्हें आज तक पहले कभी नहीं देखा गया, उन्हें तुम देखो। चराचर-सहित सम्पूर्ण जगत् को भी इस मेरे शरीर में अवयव-रूप से एकत्र स्थित आज देख लो तथा अन्य जो कुछ भी देखना चाहते हो, वह भी देख लो।"
अर्जुन को अपने चर्म-चक्षुओं द्वारा उस दिव्य रूप को देखने में असमर्थ पा कर के भगवान् ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की।
संजय, जो युद्ध-क्षेत्र में चल रही सभी घटनाओं को प्रत्यक्ष देख रहे थे, अब अर्जुन को श्रीकृष्ण ने अपना जो दिव्य रूप दिखाया था, उसका धृतराष्ट्र के सम्मुख वर्णन करते हैं।
श्रीकृष्ण भगवान् के उस विराट् स्वरूप में अर्जुन ने नाना विभागों में स्थित समस्त जगत् का दर्शन किया। उसमें हजारों अवयवों सहित सभी दिशाओं की ओर मुखाकृतियों, अनेक मुख और उदरों से युक्त, मालाओं तथा आभूषणों को धारण किये हुए तथा शस्त्रों को हाथों में उठाये हुए रूप को उन्होंने देखा। उस विराट् स्वरूप के सूर्य और चन्द्र मुख्य नेत्र थे। आकाश में हजारों सूर्यों के एक-साथ उदित होने पर जैसा प्रकाश हो वैसे प्रकाश से भगवान् प्रकाशित थे। ऐसा अद्भुत दिव्य रूप देख कर अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार कर कहा: "मैं आपको जिनके अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्र हैं, ऐसा सब ओर से देख रहा हूँ। मैं कमलासन पर स्थित ब्रह्मा, शिव तथा सभी ऋषियों, एकादश रुद्रों, द्वादश आदित्यों, आठ वसुओं, साध्यों, विश्वेदेवों, अश्विनीकुमारों, मरुद्गणों, पितरों तथा गन्धर्वो, यक्षों, असुरों और सिद्धों के समुदाय को देख रहा हूँ जो सब-के-सब विस्मित हुए आपको देख रहे हैं। आपके अनेक मुखों से अग्नि की लपटें बाहर निकल रही हैं। अनेक दाँतों वाले इस भयंकर रूप को देख कर सभी लोक भयभीत हो रहे हैं। अनेक वर्णों से प्रकाशित इस दिव्य रूप को, आकाश को स्पर्श करते हुए एवं फैले हुए विशाल मुखों को देख कर वहाँ एकत्रित कौरवों सहित पृथ्वी के असंख्य राजा, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि आपके प्रखर प्रज्वलित मुखों में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं मानो समुद्र में नदियाँ प्रवेश कर रही हों। उनमें से कुछ तो आपके दाँतों के दराजों में चिपके हुए हैं और उनका शिर चकनाचूर हो रहा है। प्रज्वलित अग्नि में जैसे अपने विनाश के लिए पतंगे वेग के साथ दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही ये सब योद्धा लोग भी आपके प्रदीप्त मुखों में बड़े वेग के साथ प्रविष्ट हो रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों से उन सबको सभी ओर से अपना ग्रास बनाते हुए चाटे जा रहे हैं। आपकी प्रभाएँ समस्त संसार को व्याप्त कर अपने उग्र तेज से उसे सन्तप्त कर रही हैं।"
तब अर्जुन ने पूछा: "ऐसे उग्र रूप वाले आप कौन हैं, यह मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि यह रूप आपने किस प्रयोजन से धारण किया है?"
इस पर भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा "मैं विश्व का विनाश करने वाला अति-उग्र काल हूँ और लोकों का संहार करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध किये बिना भी शत्रु-पक्ष के ये सभी योद्धा जीवित नहीं बचेंगे। कौरव-दल के भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण आदि सभी वीर योद्धाओं को मैं मार चुका हूँ। मैंने उनका विनाश कर डाला है। तुम केवल इसके निमित्त मात्र बन कर विजय प्राप्त करो और समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो।"
अब संजय अर्जुन की अवस्था और सर्वशक्तिमान् प्रभु से उन्होंने जो प्रार्थना की, उसका वर्णन करते हैं।
अर्जुन दोनों हाथ जोड़ कर काँपते हुए नतमस्तक हो भगवान् को प्रणाम कर गद्गद कण्ठ से प्रभु से बोले : "आपके भक्त संसार में आपका नाम, यश और विभूतियों का गान करते हुए आनन्दमग्न हो रहे हैं, जब कि दुष्ट प्रकृति वाले राक्षस भयभीत हो नाना दिशाओं में भाग रहे हैं, सिद्धों के सभी समूह आपको प्रणाम कर रहे हैं।"
भगवान् श्रीकृष्ण के विश्वरूप को देख कर अर्जुन ने कहा : "हे महात्मन्! ये दुष्ट लोग आपको प्रणाम क्यों न करें; क्योंकि आप सबसे अधिक महान् हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भी आप आदि कारण हैं। हे देवेश! हे जगन्निवास ! आप व्यक्त तथा अव्यक्त तथा उनसे भी परे अक्षर ब्रह्म हैं। आप आदिदेव हैं, पुराण पुरुष हैं, विश्व के परम आश्रय-स्थान हैं तथा ज्ञाता, ज्ञेय और परम धाम हैं। आप अपने रूपों को धारण कर विश्व में व्यापे हुए हैं। आप ही वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, ब्रह्मा तथा प्रपितामह हैं। हे भगवान्! आपको बार-बार प्रणाम है। मैं पुनः पुनः सहस्रों बार आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको आगे, पीछे तथा सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। हे अनन्त सामर्थ्य तथा अमित पराक्रम वाले ! आप समस्त विश्व को व्याप्त किये हुए हैं; इसलिए आप सर्वरूप हैं। मैंने आपकी महिमा न जानते हुए असावधानी, प्रमाद या प्रेम के वशीभूत हो आपको अकेले में अथवा मित्रों के बीच सखा मान कर 'हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा' आदि शब्दों से सम्बोधित किया है, इसके लिए हे अप्रमेय स्वरूप ! मुझे क्षमा कीजिए। यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आप इस चराचर जगत् के पिता हैं। आप इस लोक-समुदाय में पूजनीय और पूज्य गुरु हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में जब आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे अधिक दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है? इसलिए हे आराध्य देव। मैं आपको नत-मस्तक हो साष्टांग नमस्कार कर आपसे क्षमा-याचना करता हूँ। हे भगवान्' जैसे पिता पुत्र को, मित्र अपने सखा को, प्रियतम प्रिया को क्षमा कर देते हैं वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैंने पूर्व में कभी न देखा हुआ आपका अलौकिक रूप आज देखा और इससे मुझे परम हर्ष हुआ है; परन्तु मेरा हृदय भय से काँप रहा है। मैं अब पुन दिव्य मुकुट, गदा तथा सुदर्शनचक्र-युक्त चतुर्भुज रूप में आपको देखना चाहता हूँ। आपके इस विराट् विश्वरूप को देखने की शक्ति तथा साहस मुझमें नहीं है।"
इस पर भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा "हे अर्जुन, मैंने अपना यह परम रूप केवल तुम्हें ही अपनी योग-शक्ति के प्रभाव से दिखाया है। आज तक इस मर्त्यलोक में किसी ने इस स्वरूप को नहीं देखा। इस विश्वरूप का दर्शन शास्त्रों के अभ्यास से, क्रियाकर्मों से, दान से अथवा उग्र तपश्चर्या से नहीं हो सकता। केवल मेरी एकाग्र मन से भक्ति करने वाला ही इसे देख सकता है।"
संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि बाद में श्रीकृष्ण भगवान् ने पुनः अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे कर उनको आश्वस्त किया।
श्रीकृष्ण ने अर्जुन की इच्छा परिपूर्ण कर उन्हें बतलाया कि उनके इस रूप का दर्शन अन्य लोगों के लिए अत्यन्त दुर्लभ है। देवता गण भी उनके इस रूप को देखने के लिए आतुर रहते हैं। वेद के अध्ययन से, दान से, तप या यज्ञादि से भगवान् के दर्शन नहीं हो सकते। केवल एकाग्र भक्ति से ही उन्हें जानना, देखना तथा उनमें लीन होना सम्भव है। जो अपने सभी काम निष्काम भाव से, ईश्वरार्पण बुद्धि से केवल मुझको ही सर्वोच्च मान कर करते हैं, जो भक्ति-भाव से मुझमें तन्मय रहते हैं, जिन्हें अन्य किसी वस्तु की चाह नहीं है और जो किसी भी प्राणी के प्रति वैर-भाव नहीं रखते, ऐसे भक्त ही मुझे पा सकते हैं।
इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि सर्वशक्तिमान् परमात्मा का विश्वरूप चर्म-चक्षुओं द्वारा देख सकना असम्भव है। मन को सम्पूर्ण रूप से पवित्र बनाये बिना यदि कोई विश्वरूप का दर्शन करेगा तो अर्जुन के समान ही उसे भारी आघात लगेगा। भगवान् कहते हैं कि सब साधक सामान्य रूप से जैसा करते हैं, उस प्रकार के केवल शास्त्राभ्यास से, तप से, दान से अथवा यज्ञ से उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। केवल निष्ठा वाली अनन्य भक्ति के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है, देखा जा सकता है तथा गम्भीर ध्यान में शुद्ध तथा निर्दोष अन्तःकरण द्वारा उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। भगवान् पुन बल देते हुए कहते हैं कि सर्वशक्तिमान् प्रभु में अटूट श्रद्धा तथा उनका भक्तिपूर्वक ध्यान ही भगवद्-चेतना प्राप्त करने एवं मानव का अज्ञान दूर करने का एकमात्र साधन है। इसीलिए मुनि गण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहता हुआ भगवद्-साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आकांक्षित योग्यता सांसारिक पद या वैभव नहीं अपितु श्रद्धा, भक्ति और अविरत ध्यान है।
इस प्रकार 'विश्वरूपदर्शनयोग' नामक यह एकादश अध्याय समाप्त होता है।
द्वादश अध्याय
भक्तियोग
पिछले अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था कि जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात् भगवद्-साक्षात्कार को प्राप्त करना अनन्य भक्ति के द्वारा ही सम्भव है। भगवान् ने सगुण और निर्गुण-इन दोनों प्रकार की भक्तियों का निरूपण किया है। अब अर्जुन श्रीकृष्ण से पूछते हैं कि किस प्रकार का भक्त श्रेष्ठ योगवेत्ता है।
श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो भक्त गम्भीर तथा परम श्रद्धा से भगवान् को सबका स्वामी और योगेश्वर मान कर उनके विश्वरूप में सदा अपना मन एकाग्र करता है और जो सब प्रकार की कामनाओं और दुर्वासनाओं से मुक्त रहता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। जो अपनी सभी इन्द्रियों का संयम कर लेता है, सदैव समत्व बुद्धि रखता है, सब प्राणियों के कल्याण में रत रहता है, वह भी भगवद्-साक्षात्कार पा लेता है। भगवान् कहते हैं कि सगुण तथा निर्गुण, उभय प्रकार की उपासना करने वाले भक्त भगवान् के समीप पहुँच जाते हैं। अव्यक्त की उपासना कठिन है, पर वह शीघ्र परिणामदायक है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक को प्रारम्भ से ही अपने शरीर का लेश मात्र भी मोह नहीं होना चाहिए।
भगवान् कहते हैं: "हे अर्जुन! तुम भी मेरे विश्वरूप में अपने मन और बुद्धि को स्थिर करो। ऐसा करने से तुम मेरे ही रूप से मुझमें निवास कर करोगे। यदि यह तुम्हारे लिए सम्भव न हो तो योग के सतत अभ्यास से मुझमें मन को स्थिर करो। यदि इसमें भी तुम असमर्थ हो तो तुम मत्कर्मपरायण हो कर केवल उनके साक्षी बने रहो। इससे तुम पूर्णता को प्राप्त कर सकोगे। यदि मेरे लिए कर्म करना असम्भव प्रतीत हो तो मेरी शरण ले कर कर्म-फल मुझे अर्पण कर दो।"
भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन की सहायता करने के लिए अनेक युक्तियाँ बताते हैं जिससे वह उनमें से एक को पसन्द कर उसके अनुसार आचरण द्वारा भगवद्-साक्षात्कार कर सके। भगवान् कहते हैं कि अभ्यासयोग की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। सैद्धान्तिक परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। (कर्म-फल का) त्याग ध्यान से श्रेष्ठ है। ध्यान में एकाग्र हो कर परम तत्त्व का अविरत चिन्तन करना पड़ता है। भगवान् कहते हैं कि कर्म-फल के त्याग से मनुष्य परम शान्ति (वैश्व चैतन्य) पा सकता है। अब जिसने मानसिक शान्ति प्राप्त कर भगवद्-साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे भक्त के लक्षणों का भगवान् वर्णन करते हैं।
"जो मनुष्य किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबके साथ मैत्री और करुणा-भाव रखता है, जो ममता और अहंकार से रहित है, सुख-दुःख में सन्तुलित रहता है, सदा सन्तुष्ट है, समाहित चित्त है, अपने मन और बुद्धि को मुझमें अर्पण कर दिया है, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे संसार को उद्वेग नहीं होता और जो संसार से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष, अमर्ष और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझको प्यारा है। जो निःस्पृह है, अन्तर्बाह्य शुद्ध, प्रत्येक कार्य में निपुण, पक्षपात-रहित, व्यथाशून्य तथा सभी सकाम कर्मों के आरम्भों का त्याग करने वाला है, वह मुझे प्रिय है। जो मित्र तथा शत्रु को सम भाव से देखता है, जिसे सद् और असद्, मान और अपमान, शीत और उष्ण आदि परस्पर विरोधी अनुभव समान प्रतीत होते हैं और जो पूर्ण भक्तियुक्त है, ऐसा व्यक्ति मुझको प्रिय है। जो निन्दा और स्तुति को समान मानता है, जो मौनी है, जीवन-निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाये उसी में सन्तुष्ट है, जिसे अपने निवास स्थान में भी कोई ममता अथवा स्वामित्व-भावना नहीं है, जो ध्यान में पूर्णतः निमग्न रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है।"
भगवान् श्रीकृष्ण भगवद्-चेतना में मग्न पुरुष का उपर्युक्त रूप में वर्णन करते हैं और जिस अमृत-रूप धर्म द्वारा ऋषियों ने सर्व-सत्ताधीश परम ध्येय-स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है, उस धर्म का अनुसरण करने की मानव मात्र को प्रेरणा देते हैं।
इस अध्याय में भगवान् मानव जाति को अमृत-स्वरूप धर्म का आचरण करने की शिक्षा देते हैं। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को ईश्वर के समीप पहुँचा दे। जब लोग अधर्माचरण करते हैं तब वे दुःख पाते हैं और जब धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं तब आजीवन सुखी और सन्तुलित रहते हैं। परमानन्द की दिशा में उद्विकास की प्रक्रिया में उनके जीवन का प्रत्येक अंग अन्य अंगों के साथ सामंजस्यपूर्ण बन जाता है। यदि मनुष्य जीवन में धर्म का आचरण करे तो उसे भौतिक एवं आध्यात्मिक-दोनों क्षेत्रों में परम आनन्द प्राप्त होता है; क्योंकि इससे आन्तर तथा बाह्य जीवन में समन्वय सध जाता है। पिछले अध्याय में भगवान् ने अर्जुन को जो अस्थिर दिव्य दर्शन कराया था, उसका यदि सतत अनुभव लेना हो तो उसके लिए चार प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास-ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म-इस अध्याय में निर्धारित किये हैं। जब पूर्णयोग की इस विधि से सतत दर्शन होने लगता है तब इस अध्याय में वर्णन किये अनुसार व्यक्ति भगवद्-भक्त बनता है।
इस प्रकार यह 'भक्तियोग' नामक द्वादश अध्याय समाप्त होता है।
त्रयोदश अध्याय
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग
प्रथम छह अध्यायों में भगवान् श्रीकृष्ण ने कर्मयोग को और उसके पश्चात् बारहवें अध्याय तक भक्तियोग को समझाया है। अब अन्तिम छह अध्यायों में वे ज्ञानयोग का विवरण देते हैं। तेरहवें अध्याय से आरम्भ कर भगवान् अब उच्च कोटि के तात्त्विक ज्ञान का विवेचन करते हैं और वे नवीन विषय में प्रवेश करते हैं जो अतीव व्यावहारिक एवं गम्भीर रूप में अध्यात्मपरक है। बारहवें अध्याय के अन्त तक के विवेचन का स्वरूप आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक था। इस वर्गीकरण के अनुसार बारहवें अध्याय में ईश्वर के स्वरूप के विषय का उपसंहार किया गया है। भगवद्गीता के टीकाकार सामान्यतः गीता के अठारह अध्यायों के तीन विभाग करते हैं। प्रथम छह अध्यायों में जीवात्मा के सर्वशक्तिमान् ईश्वर के साथ सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है। सातवें से बारहवें अध्याय तक के छह अध्याय जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन (योग) की रीति अथवा पूर्णता का पथ बतलाते हैं। तेरहवें अध्याय से आरम्भ होने वाले अन्तिम छह अध्यायों में प्रथम तथा द्वितीय विभाग में वर्णित ज्ञान का समन्वय किया गया है।
भगवान् श्रीकृष्ण अब तक जिस विषय पर बल दे रहे थे, उसमें अचानक परिवर्तन कर व्यक्ति और समष्टि के सम्बन्धों पर जोर देते हैं। इस सन्दर्भ में वे व्यक्ति और समष्टि-दोनों के विषय में एक-साथ निर्देश करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के विविध सम्बन्धों का विश्लेषण है। ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञान द्वारा एक-दूसरे के साथ सलग्न हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के विविध सम्बन्धों के स्वरूप का वर्णन इस अध्याय का मुख्य विषय है। ज्ञाता अर्थात् जानने वाला तो ज्ञान का आलम्बन ही है, यह बतला कर भगवान् श्रीकृष्ण अपने उपदेश का प्रारम्भ इन्द्रियों को स्पर्श करने वाली सत्ता से अर्थात् स्थूल शरीर से करते हैं। इस अध्याय के कुछ विवक्षित श्लोकों के विषय की चर्चा क्रमशः ऊर्ध्वतर होती जाती है।
पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान् से सगुण और निर्गुण उपासको की तुलनात्मक श्रेष्ठता के विषय में पूछा था; पर भगवान् ने प्रश्न के एक भाग का ही उत्तर दिया था। अतः अर्जुन प्रश्न के दूसरे भाग पर पुनः प्रश्न करते हैं।
अर्जुन ने कहा- "हे केशव ! मैं प्रकृति तथा पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूँ।"
तब भगवान् कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारणभूत शरीर, जिनके द्वारा सुख-दुःख का अनुभव होता है, क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र अर्थात् शरीर मुझसे अलग है, ऐसा जो ज्ञानपूर्वक जानता है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वह अन्तर्यामी सभी क्षेत्रों का मूक साक्षी है और संसार का विषय नहीं है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ (प्रकृति, प्रकृति का विकार तथा पुरुष) का ज्ञान परम ज्ञान कहलाता है। अर्जुन में इस विषय की अधिक रुचि उत्पन्न करने के लिए भगवान् ऋषियों, वेदों और ब्रह्मसूत्रों के इस विषय पर उद्धरण दे कर उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं। भगवान् कहते हैं कि ऋषियों ने अनेक प्रकार से विविध छन्दों तथा युक्तियुक्त और निश्चयपूर्ण शब्दों में इस ज्ञान को गाया है। उन्होंने घोषित किया कि पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, दश ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ, मन, इन्द्रियों के पाँच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देह, चेतना और धृति-ये सब उस क्षेत्र (शरीर) के विकार हैं जिन्हें क्षेत्रज्ञ जानता है।
अब श्रीकृष्ण सच्चे आत्मज्ञान के नाम से विख्यात सद्गुणों का, जिनसे व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार की ओर उन्मुख होता है, वर्णन करते हैं। नम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, अदम्भ, स्थिरता, आत्म-संयम, इन्द्रिय विषयों के प्रति वैराग्य, सदाचार, निरभिमानता, निरहंकारिता, जन्म, मृत्यु, जरा एवं व्याधियों के दोषों का अनुचिन्तन, अनासक्ति, शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह आदि के प्रति निर्मोह, इष्ट तथा अनिष्ट प्रसगों में समचित्तता, अनन्य योगपूर्वक भगवान् की अव्यभिचारिणी-भक्ति, एकान्तवास, जन-सम्पर्क से अरुचि, अध्यात्म-ज्ञान में निष्ठा, तत्त्व-ज्ञान के अर्थ-रूप परमात्मा का दर्शन-यह सब सच्चा ज्ञान है और इससे विपरीत जो कुछ है, वह सब अज्ञान कहलाता है। साधक को उपर्युक्त इन सब सद्गुणों को बुद्धि तथा आत्म-विश्लेषण अथवा आत्म-जागृति द्वारा प्राप्त करना चाहिए। इन गुणों का आचरण द्विविध भाव से नहीं करना चाहिए।
अब भगवान् श्रीकृष्ण पुरुष का वर्णन करते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जान लेने से मनुष्य अमर हो जाता है। यह परब्रह्म (पुरुष) अनादि है। वह न तो सत् और न असत् ही कहा जाता है। उसके हाथ-पाँव सर्वत्र हैं। उसके नेत्र, कान, मस्तक और मुख सर्वत्र हैं और वह समस्त विश्व में व्याप्त है। उसमें सभी इन्द्रियों के विषयों के गुणों का आभास होता है, फिर भी वह इन्द्रिय-रहित अनासक्त है, सबका आधार है और प्रकृति के तीन प्रकार (सत्त्व, रज और तम) के गुणों से अतीत होते हुए भी उनका भोक्ता है। वह सभी जीवों के भीतर-बाहर रहता है। वह अचर और चर भी है। अति सूक्ष्म होने के कारण वह दुज्ञेय है, कठिनाई से जाना जाता है। वह दूर भी है और समीप भी। वह अविभक्त होते हुए भी सब प्राणियों में पृथक् पृथक्-सा रहता है। वह सब प्राणियों का सर्जक, धारक और संहारक है। वह सब ज्योतियों की ज्योति है और अन्धकार से परे है। बह ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञान का ध्येय है और सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार श्रीकृष्ण क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञान का विषय संक्षेप में समझाते हैं और अन्त में कहते हैं "मेरा भक्त इस तत्त्व को जान कर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।"
प्रारम्भ में भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के विषय में समझाते हैं। वे क्षेत्र के यथार्थ स्वरूप और उसके विकारों का विवरण देने के पश्चात् प्रसंगवश आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के गुणों का उल्लेख करते हैं, जिनको जान कर मनुष्य बुद्धिमान् बनता है। एकमात्र वस्तु जिसे पुरुष (परब्रह्म) कहते हैं, उसके सभी स्वरूपों की वे विस्तृत चर्चा करते हैं।
अब भगवान् श्रीकृष्ण सांख्य-शास्त्र के अनुसार पुरुष और प्रकृति के बीच स्थापित सम्बन्धों का वर्णन करते हैं। प्रकृति और पुरुष ईश्वर-स्वरूप होने से दोनों अनादि हैं। सभी प्रकार के विकार अथवा गुण प्रकृतिजन्य हैं। शरीर और इन्द्रियाँ प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तथा पुरुष (जीव) प्रकृति के साथ सम्बन्धित होने के कारण सुख-दुख का अनुभव करता है। प्रकृति के गुणों में आसक्ति अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेने को बाध्य करती है। शरीर में रहने वाला आत्मा सबका साक्षी, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा है। जो कोई इस गुह्य पुरुष और गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वह कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है; क्योंकि वह कर्ता-कर्म से परे चैतन्य का अनुभव करते हुए सदा परमानन्द में लीन रहता है।
श्रीकृष्ण आत्म-दर्शन के अनेक उपाय बताते हैं। प्रत्यक्-चैतन्य अथवा अहं-चैतन्य का स्थान अन्तःकरण है। कुछ लोग सजगता से अन्त करण के व्यापारों का परित्याग कर प्रगाढ़ ध्यान से आत्म-तत्त्व का दर्शन करते हैं। अन्य लोग साख्य-योग द्वारा अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन एवं बुद्धि के कार्यों के साक्षी बन कर तथा सबको प्रकृतिजन्य खेल और पुरुष (आत्मा) को कर्म-रहित जान कर जीव-चैतन्य और परम-चैतन्य के ऐक्य का अनुभव करते हैं। अन्य कुछ लोग कर्मयोग द्वारा अर्थात् उद्विकास के किसी भी स्तर पर अनासक्त भाव से अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन कर परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं और मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। जो पूर्वोक्त उपायों से अनभिज्ञ हैं, ऐसे भक्त लोग शास्त्रों एवं गुरु का आश्रय ले कर भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं, स्वयं अच्छे आचरण करते हुए दूसरों की भलाई करते हैं और किसी भी प्रकार का भेद-भाव न करते हुए दिव्य जीवन व्यतीत करते हैं, वे भी भगवद्-प्राप्ति कर लेते हैं।
श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ स्थावर-जंगम पदार्थ हैं, वे सब प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं यथार्थदर्शी व्यक्ति परमात्मा को सभी जीवों में सम भाव से स्थित देखता है। जब वस्तुओं का नाश होता है, तब भी वह परमात्मा नष्ट नहीं होता। ऐसा भक्त दूसरे को कभी दुःख नहीं देता; क्योंकि वह जानता है कि उसकी अपनी आत्मा ही सबमें व्याप्त है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा अकर्ता है, प्रकृति ही सम्पूर्ण कार्य करती है तथा पृथक् पृथक् भाव से समस्त प्राणियों में एक आत्मा अवस्थित है तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है।
भगवान् कहते हैं "हे अर्जुन ! परमात्मा अविनाशी है; आदि, अन्त और गुणों से रहित है। वह शरीर में रहते हुए भी कर्म नहीं करता और न कर्म में लिप्त ही होता है।" जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में व्याप्त आकाश उनके गुणों से लिपायमान् नहीं होता, वैसे ही पुरुष (जीव) प्रकृति में (शरीर में) रहते हुए भी उसके गुणों से अलिप्त रहता है। जिस प्रकार एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो अपने ज्ञान-चक्षुओं द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथार्थ भेद को जान लेता है तथा यह भी जानता है कि सभी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, वह परम-पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है।
इस अध्याय में भगवान् यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य को साक्षी बन कर रहना चाहिए तथा विवेकपूर्वक यह समझ लेना चाहिए कि संसार की सब वस्तुएँ प्रकृति और पुरुष (जीव) के संयोग से उत्पन्न हुई हैं। मनुष्य को अपनी बुद्धि, मन, इन्द्रियों और शरीर के कार्यों के साथ अपने को तादात्म्य नहीं करना चाहिए। जैसे पृथ्वी पर गिरा हुआ वर्षा का जल मिट्टी के साथ मिल कर कीचड़ बन जाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने स्वरूप को प्रकृति-जनित पदार्थों से दूषित नहीं होने देना चाहिए।
इस प्रकार 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग' नामक यह त्रयोदश अध्याय समाप्त होता है।
चतुर्दश अध्याय
गुणत्रयविभागयोग
इस अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण प्रकृति के गुणों का वर्णन करते हैं। वे (गुण) मनुष्य को कैसे बन्धन में डालते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, उनसे व्यक्ति कैसे छुटकारा पा सकता है और इस प्रकार मुक्त हुए व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, इन सबको इस अध्याय में भगवान् बतलाते हैं।
पिछले अध्याय में भगवान् ने कहा कि पुरुष और प्रकृति का एक-साथ ही परमात्मा से प्रादुर्भाव हुआ है; अतः वे दोनों शाश्वत हैं। यहाँ श्रीकृष्ण मानव-मन को बोधगम्य विधि से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। महत् ब्रह्म मूल-प्रकृति है और सब प्राणियों की योनि है, जिसके भीतर भगवान् सभी जीवों का बीज वपन करते हैं। इस प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं।
भगवान् कहते हैं कि सत्त्व, रज और तम-ये प्रकृति के तीन गुण हैं जो जीवात्मा को शरीर के साथ बाँधे हुए हैं। इनमें सत्त्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश तथा स्वास्थ्य प्रदान करता है। वह सुख और ज्ञान द्वारा जीव को शरीर के साथ बन्धनग्रस्त बनाता है। कामना और आसक्ति से उत्पन्न रजोगुण कर्मों और उनके फलों की आसक्ति द्वारा जीव को बन्धन में डालता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और सब जीवों को भ्रान्ति में डालता है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा को उपजा कर जीव को शरीर के साथ आबद्ध करता है।
रजोगुण और सत्त्वगुण को दबा कर तमोगुण अपना वर्चस्व जमाता है। तमोगुण और सत्त्वगुण को दबा कर रजोगुण प्रबल होता है एवं रजोगुण तथा तमोगुण को दबाने से सत्त्वगुण का वर्चस्व बढ़ता है। जब अन्तःकरण तथा इन्द्रियों द्वारा ज्ञान-रूप प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सत्त्वगुण का उदय होना समझना चाहिए। जब लोभ, प्रवृत्ति, कर्मारम्भ, अशान्ति तथा विषय-भोगों की लालसा का उदय हो, तब रजोगुण की वृद्धि जाननी चाहिए और तमोगुण के उदय होने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं।
भगवान् कहते हैं कि सत्त्वगुण की वृद्धि के समय मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव उस निर्मल स्वर्गलोक में पहुँचता है जहाँ उत्तम कर्म करने वाले लोग जाते हैं। रजोगुण के वृद्धि-काल में मृत्यु को प्राप्त होने पर कर्म में आसक्ति वाले लोगों में उत्पन्न होता है और मृत्यु के समय जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है ऐसा मनुष्य मरणोपरान्त (कीड़ा, पशु आदि) मूढ़ योनियों में जन्म ग्रहण करता है।
भगवान् शिक्षा देते हैं कि सार-असार को समझते हुए सुकर्म द्वारा रजोगुण और तमोगुण को हटा कर सत्त्वगुण में स्थित हुआ जा सकता है। इसके लिए निष्काम सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, भगवन्नाम जप और ध्यानाभ्यास करना चाहिए। अन्त में भगवान् की अव्यभिचारिणी-भक्ति द्वारा सत्त्वगुण को भी छोड़ देना चाहिए। जब व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब वह जन्म-मृत्यु, जरा और दुःखों से मुक्त हो कर अमरता को प्राप्त कर लेता है।
इन तीनों गुणों से परे कैसे हुआ जा सकता है और त्रिगुणातीत पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् कहते हैं कि जो मनुष्य निश्चल भक्ति से परमात्मा को भजता है, वह गुणों को अतिक्रमण कर परमात्मा के साथ एकीभाव साध लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष सत्त्वगुण के कार्य-रूप प्रकाश के, रजोगुण के कार्य-रूप प्रवृत्ति के तथा तमोगुण के कार्य-रूप मोह के प्रवृत्त होने पर न तो द्वेष करता है और न उनसे निवृत्त होने की आकांक्षा ही करता है। वह तो परमात्मा के साथ ऐक्य-सम्पादन कर सब प्रवृत्तियों में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जान कर साक्षी के सदृश्य स्थित रहता है। वह शत्रु या मित्र, पत्थर या सोना, मान या अपमान सबको समान समझता है। वह कर्तापन का अभिमान छोड़ कर सर्वशक्तिमान् प्रभु के हाथ का एक उपकरण बन कर संसार में व्यवहार करता है और ब्रह्मपद पाने का अधिकारी होता है।
इस अध्याय में मानव-जाति को प्रकृति के तीन गुणों के मुख्य लक्षणों का भगवान् वर्णन करते हैं और उनके बन्धनों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, इसकी रीति बताते हैं। प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम, ध्यान, निष्काम कर्म आदि के द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। इसके साथ ही भगवान् ब्रह्म में एकीभाव प्राप्त पुरुष के लक्षण बताते हुए ब्रह्मपद-प्राप्ति का उपाय भी समझाते हैं।
इस प्रकार 'गुणत्रयविभागयोग' नामक यह चतुर्दश अध्याय समाप्त होता है।
पंचदश अध्याय
पुरुषोत्तमयोग
श्रीकृष्ण अपने प्रति अनन्य भक्ति के विश्वास के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का एक बार पुनः वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वैराग्य और आत्म-समर्पण द्वारा मनुष्य गुणातीत बन सकता है। वे संसार की पीपल के वृक्ष से तुलना करते हैं, जिसकी जड़ परमेश्वर में स्थित है और जिसकी शाखाएँ विश्व-विधाता ब्रह्मा हैं, जिसके पत्ते वेद हैं, जो भगवान् और सृष्टि का गुणगान करते हैं। मानव शरीर की भी वृक्ष के साथ तुलना की गयी है। ऊपर मस्तिष्क जिसका ऊर्ध्वमूल है और मेरुदण्ड को सीधा रखने वाली स्नायु-प्रणाली उसका तना है। भिन्न-भिन्न अनेक नाड़ियाँ नीचे की ओर फैल कर शरीर के सारे अवयवों को अनुस्यूत किये हैं। इस वृक्ष का पोषण तीनों गुणों से होता है। इन्द्रियों के विषय ऊपर-नीचे सर्वत्र फैले हुए उसके पल्लव तथा कोपलें हैं और कर्म उसके मूल हैं। यह बन्धन-वृक्ष दृढ़ वैराग्य-रूपी शस्त्र से काटा जा सकता है। उसके पश्चात् ही अभिमान, कर्तापन एवं मोह से व्यक्ति की मुक्ति होती है और वह सुख-दुःख के द्वन्द्वों से भी छूट जाता है। मनुष्य इस प्रकार अविनाशी परम पद को पा सकता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि यह परम पद स्वयं-प्रकाश है। उसे सूर्य, चन्द्र, तारे या अग्नि प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब उसके अंश मात्र से प्रकाशित हैं। वैराग्य और ज्ञान की तलवार से अपने अहंकार को काट कर ज्ञानी जन इस मर्त्यलोक में पुनः कभी लौट कर नहीं आते।
अब श्रीकृष्ण इस मर्त्यलोक में जीवात्मा के जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा का एक अंश ही इस देह में जीवात्मा बन कर आता है, जो मन और पंचेन्द्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ शरीर में स्थित रहता है। शरीर में रहते हुए जीवात्मा ज्ञानेन्द्रियों द्वारा संसार के विषयों का सेवन करता है और इस शरीर द्वारा अपनी अमुक वासनाओं की पूर्ति करने के बाद शरीर को त्याग देता है। उस समय वह मन तथा इन्द्रियों को अपने साथ वैसे ही ले जाता है जैसे वायु फूलों की सुगन्ध ग्रहण करके ले जाती है। अज्ञानी बोध के अभाव से आत्मा को शरीर मान लेता है और सुख-दुःख भोगता रहता है, जब कि ज्ञानी अपनी बोध-शक्ति (विवेक) से सभी प्रवृत्तियों का साक्षी मात्र बन कर रहता है। योगी जन तो भगवान् को अपने भीतर ही बैठा हुआ देखते हैं; परन्तु अज्ञानी इच्छाओं के वशीभूत होने के कारण प्रयत्न करने पर भी उन भगवान् के दर्शन नहीं कर पाते।
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि केवल उनके कारण ही सूर्य, चन्द्र, तारा गण एवं अग्नि में प्रकाश है। पृथ्वी में प्रवेश करके वे अपनी शक्ति से सभी जीवों को धारण करते हैं तथा रस-स्वरूप चन्द्रमा बन कर सभी वनस्पतियों का पोषण करते हैं। वे ही (१) भक्ष्य अर्थात् रोटी, चावल आदि ठोस आहार, (२) भोज्य अर्थात् दूध, दही आदि, (३) लेख अर्थात् मधु आदि चाटने योग्य द्रव तथा (४) चोष्य अर्थात् गन्ने, आम आदि जैसे रस चूसने योग्य पदार्थ-इन चार प्रकार के भोजनों को सभी जीवों के प्राण और अपान की संयुक्त शक्ति से पचाते हैं। भगवान् सबके हृदय में वास करते हैं और उनके द्वारा ही जीवों को स्मृति तथा ज्ञान की प्राप्ति या अप्राप्ति होती है। परमात्मा वेदों द्वारा जाने जा सकते हैं और वे ही वेदों के कर्ता तथा ज्ञाता भी हैं। जगत् में क्षर और अक्षर-दो प्रकार के पुरुष हैं। परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पोषण करते हैं। वे क्षर तथा अक्षर से परे हैं; इसलिए वेदों में उन्हें 'पुरुषोत्तम' कहा गया है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति उन्हें पुरुषोत्तम-रूप में जानता है, वह सब प्रकार से उनको ही निरन्तर भजता है। इस प्रकार जगत् में अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन कर भगवान् अर्जुन तथा समस्त मानव-जाति को यह उपदेश देते हैं कि इस गोपनीय ज्ञान को जान कर वह जीवन के परम ध्येय अर्थात् ईश्वर-साक्षात्कार को प्राप्त कर ज्ञानवान् हो जाये।
इस अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण बतलाते हैं कि सब नाम-रूपों में, संसार के सभी चर-अचर पदार्थों में वे ही समाविष्ट हैं। उनकी शक्ति के अंश मात्र से सूर्य, चन्द्र, ताराओं सहित सभी ग्रह भ्रमण कर रहे हैं और प्रकाशित हैं। एकमात्र भगवान् ही चैतन्य-रूप से मानव-जीवन के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य सभी स्तरों पर विराजमान हैं। भगवान् कहते हैं कि जो निर्मोह-चित्त हो कर मुझे पुरुषोत्तम-रूप में जानता है, वही सर्वज्ञ है एवं वही सर्वात्मना मुझे भजता है। जो इस गुह्यातिगुह्य ज्ञान को जानता है, वह ज्ञानवान् हो जाता है, उसके सभी सन्देहों तथा इस संसार के शोक-ताप का शीघ्र अन्त हो जाता है और वह कृतकृत्य हो जाता है।
इस भाँति 'पुरुषोत्तमयोग' नामक यह पंचदश अध्याय यहाँ समाप्त होता है।
षोडश अध्याय
दैवासुरसम्पद्विभागयोग
मनुष्य सद् और असद् का मिश्रण है। वह बुद्धि के सम्यक् उपयोग से दिव्य बन सकता है। ज्ञानी जन अपनी दैवी प्रकृति के कारण भगवान् को पुरुषोत्तम-रूप में जान कर पूर्ण हृदय से उनको भजते हैं। अज्ञानी जन वासनाओं के कारण आसुरी स्वभाव के होते हैं। वे सांसारिक विषयों में सुख की खोज करते हैं और उनमें विराजमान भगवान् की उपस्थिति अनुभव करना भूल जाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण मानव-जाति को उसके जीवनोद्देश्य की प्राप्ति के सम्यक् मार्ग का दिग्दर्शन करने तथा सत् और असत् में विवेक करने की शिक्षा देने के लिए दैवी और आसुरी प्रकृति का वर्णन करते हैं।
भगवान् कहते हैं कि मुमुक्षु में अभय, अन्तःकरण की शुद्धता, तत्त्वज्ञान के लिए ध्यानयोग में मन की निरन्तर दृढ़ स्थित, सात्त्विक दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, सरलता, अहिंसा, सत्य, उत्तेजना में भी अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपिशुनता, समस्त प्राणियों के प्रति दया, अलोलुपता, कोमलता, लज्जा, अचपलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अद्रोह, अनभिमानता आदि दिव्य गुण होते हैं।
आसुरी प्रकृति में जन्म लेने वाले पुरुष दम्भ, अहंकार, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान जैसी आसुरी सम्पद् को प्राप्त होते हैं।
दैवी गुणों के आचरण से मनुष्य संसार-बन्धन से आत्यन्तिक मुक्ति को प्राप्त कर परम आनन्द का लाभ लेता है। आसुरी गुणों के आश्रय से मनुष्य बन्धन तथा कष्ट में पड़ता है।
भगवान् श्रीकृष्ण मनुष्य की आसुरी प्रकृति के गुणों का और आगे वर्णन करते हैं। आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी मनुष्यों में धर्माधर्म का ज्ञान नहीं होता। उनमें शौच नहीं होता, आचार नहीं होता और न सत्य ही होता है। वे ऐसा मानते हैं कि यह जगत् मिथ्या, आश्रय-रहित, स्रष्टा तथा व्यवस्थापक ईश्वर से हीन है तथा कामनासक्त पुरुष और स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इन मिथ्या विचारों का आश्रय ले कर विकृत स्वभाव वाले अल्पज्ञ क्रूरकर्मी मनुष्य मानव-जाति तथा समस्त जगत् के लिए विनाशकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति नाम, यश और अधिकार की दुष्पूरणीय कामना से युक्त हो कर दम्भ, अभिमान और मद से मत्त अज्ञानवश अशुभ सिद्धान्तों को ग्रहण कर वेद-विरुद्ध कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे कामनाओं की पूर्ति के लिए विलासपूर्ण साधनों के संग्रह तथा विषय-भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्ण उपायों से धनसंचय कर काम तथा क्रोध के दास बन जाते हैं और यह मानते हैं कि यही उनका जीवन-सर्वस्व है। वे अपने-आपसे कहते हैं- 'आज मुझे यह प्राप्त हुआ। इतना धन मेरे पास हो गया। अब भविष्य में और भी धन प्राप्त करूँगा। मैंने अनेक को हराया है और अब तक जिनको मैं अपने वश में नहीं कर पाया हूँ उन्हें भी वश में कर लूँगा' आदि-आदि। अनेक प्रकार की कल्पनाओं से भ्रमित चित्त वाले, मायाजाल में फंसे हुए विषय-भोगों में आसक्त अज्ञानी जन घोर नरक में गिरते हैं। धन और मान के मद से युक्त और दम्भ से भरे हुए ये नाम और कीर्ति के लिए शास्त्र-विधि के विपरीत कर्म करते हैं। अहंकार, बल, दर्प, कामना और क्रोध के कारण ये दूसरों की निन्दा करने वाले लोग अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित भगवान् से द्वेष करते हैं। भगवान् कहते हैं कि मेरे अटल नियम ऐसे पापाचारी नराधमों को जन्म-मरण के चक्र द्वारा आसुरी योनियों में डाल देते हैं। वे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्म आसुरी योनियों को प्राप्त हुए ईश्वर-प्राप्ति न कर पशु आदि से भी अधिक नीच योनियों में जन्म लेते हैं।
भगवान् कहते हैं-"यह सब जान कर मनुष्य को नरक की प्राप्ति में हेतुभूत काम, क्रोध एवं लोभ को त्याग देना चाहिए और शास्त्र को प्रमाण मान कर ऋषियों एवं सन्तों द्वारा बताये हुए मार्ग पर निष्ठापूर्वक आचरण करना चाहिए। इससे व्यक्ति को परम गति प्राप्त होती है। परन्तु जो व्यक्ति शास्त्र-विधि त्याग कर स्वेच्छाचारी हो कार्य करता है, वह न तो सिद्धि को, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। अतः कर्तव्य और अकर्तव्य के निरूपण में एक शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण है, ऐसा जान कर तू शास्त्रविधानोक्त कर्म ही करने योग्य है।"
इस अध्याय में बताया गया है कि सब लोगों को आत्म-विश्लेषण कर अपने चारित्र्य में भरे हुए अवांछनीय गुणों को खोज कर विवेक और अन्तरावलोकन द्वारा उनको तत्काल दूर करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें अपने प्रति पूर्णतः प्रामाणिक रह कर मन के कार्य-कलापों का साक्षी बनना होगा। इस स्थिति में ही व्यक्ति को यह पता चल सकेगा कि अमुक विचार अथवा कर्म उसके लिए कल्याणप्रद है अथवा नहीं। इस अध्याय में बतायी गयी दैवी और आसुरी सम्पत्तियाँ सामान्य अर्थ में भली या बुरी नहीं है। इनमें नैतिक दृष्टिकोण के गुणों-अवगुणों से कहीं अधिक गम्भीर तात्त्विक अर्थ समाविष्ट है। यहाँ इस द्वन्द्व के सिद्धान्त की तत्त्वज्ञान से तुलना कर सदा के लिए उसका निर्णय कर दिया है। जगत् परमात्मा का शरीर है। इस पूर्ण विश्व-सत्ता में देवासुर संग्राम नहीं हो सकता। इस संघर्ष को जीत कर शुद्ध सत्त्व का विश्वात्म-भाव कार्यशील होता है।
इस प्रकार 'दैवासुरसम्पद्विभागयोग' नामक यह षोडश अध्याय समाप्त होता है।
सप्तदश अध्याय
श्रद्धात्रयविभागयोग
शास्त्र को ही प्रमाण मान कर चलने तथा शास्त्रोक्त व्यवस्था से नियत कर्म करने की भगवान् श्रीकृष्ण की अनुज्ञा सुन कर अर्जुन ने पूछा कि जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि परित्याग कर श्रद्धापूर्वक देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी क्या दशा होती है? इस पर भगवान् श्रद्धा के तीन विभाग कर कहते हैं कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही मनुष्य का स्वरूप निर्धारित करती है। सात्त्विक, राजसिक और तामसिक- ये तीनों ही प्रकार के लोग भगवान् को पूजते हैं; परन्तु उसका फल तो उनकी श्रद्धा के अनुसार ही मिलता है। सात्त्विक मनुष्य देवों की, राजसिक मनुष्य यक्ष और राक्षसों की तथा तामसिक जन भूत-प्रेतों की पूजा करते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो लोग काम, लोभ तथा क्रोध का परित्याग किये बिना, तप के नाम पर शास्त्रविधि-रहित उग्र तपस्या कर शरीर को कष्ट देते हैं, उनकी श्रद्धा राजसिक है। अविवेकी होने के कारण वे शरीर-स्थित भूत-समूह को और हृदय में निवास करने वाले मुझ अन्तर्यामी को भी कृश करते हैं। ऐसे लोगों को आसुरी स्वभाव वाले समझना चाहिए।
कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं सात्त्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार सबके प्रिय आहार-सहित यज्ञ, दान और तप के भी तीन भेद किये गये हैं। जो आहार आयु, सत्त्व, बल, आरोग्य, सुख और आनन्दवर्धक, सरस, स्निग्ध, पौष्टिक और मन को प्रिय हो, वह सात्त्विक आहार कहलाता है। दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला, कडुआ, खट्टा, नमकीन, अति-गरम, तीखा, सूखा और प्रदाहकारक आहार राजसिक लोगों को प्रिय होता है। दूषित, स्वाद-रहित, दुर्गन्धयुक्त, बासी और अशुद्ध आहार तामसिक लोगों को अच्छा लगता है। शरीर का संवर्धन आहार पर ही निर्भर है। अतः आहार के गुण का ध्यान रखना आवश्यक है।
फल की आशा न रखते हुए शास्त्रोक्त विधि से किया गया यज्ञ सात्त्विक यज्ञ है, फल की कामना से तथा दम्भाचरण के लिए किया गया यज्ञ राजसिक कहलाता है और शास्त्रोक्त विधि का अनादर करते हुए बिना अन्नदान एवं दक्षिणा दिये बिना केवल नाम और यश के लिए किया गया यज्ञ तामसिक कहलाता है।
तप भी तीन प्रकार के होते हैं: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। देवता, वेदज्ञ, ब्राह्मण, गुरु तथा ज्ञानियों का पूजन, शौच, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि शारीरिक तप हैं। अनुद्वेगकारी, सत्य, प्रिय तथा हित-जनक सम्भाषण, स्वाध्याय, प्रभु के दिव्य नाम का जपादि वाणी-सम्बन्धी तप हैं। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन भाव, मनोनिग्रह, भाव-संशुद्धि आदि मानसिक तप हैं। ये तीनों प्रकार के तप सात्त्विक तप की श्रेणी में आते हैं। सत्कार, मान, पूजा के लिए अनुष्ठित आडम्बरपूर्ण तप राजसिक तप कहा गया है। यह अस्थिर एवं क्षणिक फल वाला है। जो तप अविवेकपूर्वक निज-शरीर को पीड़ा दे कर अथवा दूसरे प्राणियों के विनाशार्थ किया जाता है, वह तामसिक है।
दान को कर्तव्य-बोध से, प्रत्युपकार की आशा न रखते हुए देश, काल तथा पात्र की उत्तमता के विचारपूर्वक दिया गया दान सात्त्विक दान है। प्रत्युपकार की भावना से अथवा भविष्य में लाभ की आशा से दुःखी चित्त से दिया गया दान राजसिक दान है। अनुपयुक्त देश, अयोग्य काल में अपात्र को सत्कार-रहित, अवज्ञापूर्वक दिया गया दान तामसिक दान कहा गया है। ईश्वर को सन्निकट समझते हुए अपने दोषों को दूर करने के उद्देश्य से एवं सात्त्विक भावना से यज्ञ, तप तथा दान करने के लिए श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ये सभी कार्य ब्रह्म के नाम- 'ॐ तत्सत्' -के उच्चारण के साथ सम्पन्न करने चाहिए। 'ॐ' भगवान् का प्रतीक तथा वेदों का सार है। संसार की सभी वस्तुएँ भगवान् की हैं, ऐसी अनुभूति 'तत्' से होती है। इससे अहंकार तथा ममता का नाश होता है। 'मैं-पन' और 'मेरा-पन' नहीं रह जाता। 'सत्' भगवान् के शाश्वत तथा श्रेष्ठ भाव का प्रतिनिधित्व करता है और स्वार्थी प्रवृत्तियों का दमन करके मनुष्य को ईश्वर-साक्षात्कार के योग्य बनाता है।
श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अश्रद्धापूर्वक अनुष्ठित यज्ञ, तप और दान 'असत्' अर्थात् मिथ्या है और इस लोक या परलोक में फलप्रद नहीं होता।
इस अध्याय से मनुष्य को यह शिक्षा मिलती है कि सभी (शारीरिक तथा मानसिक) कर्म विवेक और श्रद्धापूर्वक सम्पन्न करने पर श्रेयदायक होते हैं।
इस प्रकार 'श्रद्धात्रयविभागयोग' नामक यह सप्तदश अध्याय समाप्त होता है।
अष्टादश अध्याय
मोक्षसंन्यासयोग
भगवान् श्रीकृष्ण का उपदेश जीवन के सर्वांगीण विकास की कला का मार्ग प्रशस्त करता है। मानव-जीवन के विकास की प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक प्रक्रम में हम कैसे रहें, कैसा व्यवहार करें और किस प्रकार विचार करें-इन सबका भगवद्गीता सम्पूर्ण रूप से मार्ग-दर्शक है। भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पालनीय आचार संहिता सहित कर्मयोग, सांख्ययोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग की शिक्षा दी। व्यावहारिक ज्ञान की इसी सम्पूर्णता ने गीता को एक अमर ग्रन्थ बना दिया है। अब तक दिये गये सारे उपदेशों के सार का समुच्चय करने के विचार से अर्जुन ने संन्यास और त्याग के यथार्थ स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की।
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों के मतानुसार काम्य कर्मों का त्याग 'संन्यास' है और समस्त कर्मों के फल का त्याग 'त्याग' है। कई विद्वान् ऐसा भी कहते हैं कि कर्म मात्र का त्याग कर देना चाहिए, जब कि कुछ अन्य मनीषियों का कथन है कि यज्ञ, दान और तप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान् श्रीकृष्ण अपना मत प्रकट करते हैं कि व्यक्ति को यज्ञ, दान और तप जैसे कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, परन्तु उनके फल का सर्वथा त्याग करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ज्ञानियों को पवित्र बनाते हैं। नियत कर्मों का त्याग करने वाला तामसिक और सभी कर्म समान रूप से दुःखदायी हैं, ऐसा सोच कर शारीरिक क्लेश के भय से स्वधर्म का पालन न करने वाला राजसिक कहा गया है। उसे उसके त्याग का फल नहीं मिलता। इच्छा और आसक्ति को छोड़ कर कर्तव्य-पालन की भावना से कर्म करने वाला सात्त्विक और बुद्धिमान् तथा सर्वसंशय-रहित होता है। उसे प्रतिकूल कर्मों से द्वेष और अनुकूल कर्मों से राग नहीं होता।
चूँकि देहाभिमानी व्यक्ति सभी कर्मों का निःशेष रूप से त्याग नहीं कर सकता, अतः कर्म-फल-त्यागी को ही त्यागी कहा जाता है। जो कर्म फल का त्याग नहीं करते, उन्हीं को ही अच्छे, बुरे या मिश्रित कर्मों का फल भोगना पड़ता है, त्यागी को नहीं। यहाँ तक भगवान् श्रीकृष्ण ने त्याग अर्थात् कर्मयोग का सच्चा अर्थ विस्तारपूर्वक समझाया। अब वे संन्यास अथवा 'सांख्ययोग' का सांख्य दर्शन के अनुसार प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म का अधिष्ठान (शरीर), कर्ता (अन्त करण), पृथक् पृथक् करण (इन्द्रियाँ), नानाविध चेष्टाएँ तथा दैव-ये कर्म की सिद्धि के पाँच कारण हैं। मनुष्य मन, बाणी अथवा शरीर से धर्म परन्तु जो व्यक्ति अज्ञानवश अपनी असंग आत्मा को कर्ता-रूप देखता है, वह असस्कृत बुद्धि वाला अज्ञानी सम्यक् रूप से नहीं देखता है। जो कर्ता-पन के अभिमान से मुक्त है. जिसकी बुद्धि कार्य में आसक्त नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति लोगों का हनन करते हुए भी हनम नहीं करता है और न (इस प्रकार के) कर्म से आबद्ध ही होता है। आत्मा अकर्ता है। पर की मलिनता के कारण अज्ञानी जन शरीर और इन्द्रियों को ही आत्मा मानते हैं और स्वय को सब कर्मों का कर्ता मानते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय-ये तीन शरीर, मन तथा वाणी के द्वारा कर्म के प्रवर्तक हैं। जिस ज्ञान द्वारा सभी प्राणियों में एक अक्षर पुरुष की उपलब्धि होती है, भगवान् श्रीकृष्ण उस ज्ञान का विवेचन करते हैं। कर्म एवं कर्ता सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणों से प्रेरित हुआ करते हैं। ईश्वर-साक्षात्कार के सहायक सात्विक गुणों के विकास के लिए व्यक्ति को ईश्वर-साक्षात्कार के प्रतिकूल प्रभावशाली राजस तथा तामस गुणों का परित्याग करना चाहिए।
जिस ज्ञान के द्वारा भिन्न-भिन्न भूत-समूह में एक सर्वव्यापक एवं अव्यय सत्ता की उपलब्धि होती है, वह सात्त्विक ज्ञान कहा गया है। जिस ज्ञान के कारण व्यक्ति भिन्न-भिन्त्र जीवों को नानाविध भाव से देखता है, वह राजसिक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान द्वारा व्यक्ति विवेक-बुद्धि का उपयोग न कर एक तथा आंशिक विषय को ही सम्पूर्ण एवं यथार्थ समझ कर रह जाता है, वह तामसिक ज्ञान कहलाता है।
शास्त्र-विहित तथा आसक्ति-विहीन भाव तथा फलाकांक्षा रहित हो कर अनुष्ठित कर्म सात्त्विक कहा गया है। सकाम भाव से अनुष्ठित कृच्छ्र साध्य काम्य कर्म राजसिक कहलाता है। जो कर्म पौरुष, भावी परिणाम, हानि, हिंसा आदि का विचार किये बिना अविवेकपूर्वक सम्पन्न किया जाता है, वह कर्म तामसिक कहा गया है।
अहंकार-शून्य, आसक्ति-विहीन, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य की सफलता-असफलता से अप्रभावित रहने वाला कर्ता सात्विक कहलाता है। विषयानुरागी, कर्मफलाकांक्षी, लोभी, हिंसापरायण, अशुचि तथा हर्ष और शोकयुक्त कर्ता राजसिक कहलाता है। असमाहित, विवेक-शून्य, उद्धत, अनम्र, बचक, आलसी, विषायुक्त तथा दीर्घसूत्री कर्ता तामसिक कहा गया है।
भगवान् श्रीकृष्ण गुणों के प्रकार-भेद से बुद्धि एवं धृति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिस बुद्धि को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, कार्य तथा अकार्य, भय और अभय एवं आत्म-बन्धन तथा मोक्ष का भेद परिज्ञात है, ऐसी बुद्धि सात्त्विक है। जिस बुद्धि द्वारा धर्म तथा अधर्म का, कार्य तथा अकार्य का असन्दिग्ध ज्ञान नहीं होता, वह राजसिक बुद्धि है।
जो बुद्धि अज्ञानावृत्त हो कर अधर्म को धर्म मानती है, वह विपरीत ज्ञान वाली होती है और तामसिक बुद्धि कहलाती है।
जो अव्यभिचारिणी धृति योग के द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रिया-शक्ति का निरोध करती है, वह सात्त्विक धृति कहलाती है। कर्तृत्वादि के अभिनिवेशपूर्वक फलाकांक्षी हो कर जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, बह धृति राजसिक है। दुर्बुद्धि व्यक्ति जिस धृति द्वारा अति-निद्रा, भय, शोक, विषाद तथा मद का परित्याग नहीं करता है, वह धृति तामसिक है।
जो सुख आरम्भ में दुःखदायी तथा परिणाम में अमृत-रूप होता है और जो आत्म-विषयिनी बुद्धि की विमलता से उत्पन्न होता है, वह सात्त्विक सुख है। जो सुख विषय तथा इन्द्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है और जो प्रथम अमृतवत्, किन्तु परिणाम में विष-तुल्य बोध होता है, वह राजसिक सुख कहलाता है। जो सुख आरम्भ में तथा परिणाम में भी बुद्धि को मोह-मुग्ध करता है तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। पृथ्वी पर या स्वर्ग में देवताओं के मध्य कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो।
मनुष्य के स्वभावज गुणों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के कर्म पृथक् पृथक् रूप से व्यवस्थित किये गये हैं। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, ऋजुता, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिक्य-ये सब ब्राह्मणों के स्वभावजात कर्म हैं। शौर्य, तेज, धैर्य, चातुर्य (युद्ध-कौशल), दान, प्रभुत्व आदि क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गोपालन और वाणिज्य वैश्यों के स्वभावज कर्म हैं। शुश्रूषा शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। जब मनुष्य अपने स्वधर्म में निष्ठापूर्वक तत्पर होता है तो वह परम सिद्धि प्राप्त करके जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुँच जाता है।
प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा और विकास-प्रक्रम के अनुसार किसी विशेष वातावरण में जन्म लेता है। इसीलिए कोई जन्म से ही निर्धन तो कोई धनवान्, कोई मन्दबुद्धि तो कोई बुद्धिमान् तथा विद्वान् होता है। ऐसा विचार कर मनुष्य को आत्म-तुष्ट होना चाहिए तथा मान, नाम, यश तथा पद के लिए नियत कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जो इस सत्य को नहीं समझता, वह अपने कर्तव्य-कर्म का पालन नहीं करेगा। अतएव भगवान् कहते हैं कि सम्यक् रूप से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा स्वधर्म का असम्यक् अनुष्ठान भी श्रेष्ठ है। स्वभाव से किये गये कर्म का सम्पादन करने से मनुष्य पापभागी नहीं होता। स्वभावजात कर्म दोषयुक्त होने पर भी उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। धूमावृत अग्नि की भाँति सभी कर्म सामान्यतः दोषावृत होते हैं।
इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण ने त्याग और संन्यास की व्याख्या कर ज्ञान-मार्ग का विवरण दिया। त्याग जिसका दूसरा नाम कर्मयोग है, उसकी तथा विभिन्न गुणों के साथ उसके स्वरूप की व्याख्या की तथा कर्मयोग के साथ भक्तियोग का सम्बन्ध दर्शाया। भगवान् ने यह भी समझाया कि दैनन्दिन जीवन में विकास के सभी प्रक्रमों में कर्मयोग का आचरण सुसाध्य है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि निष्ठापूर्वक अनुष्ठित कर्म भगवद्-साक्षात्कार-प्रदायक होता है।
भगवान् श्रीकृष्ण सांख्ययोग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसकी बुद्धि सब विषयों से अनासक्त है, जिसकी भोग की स्पृहा विगत हो चुकी है, जिसने अपने मन को पूर्ण संयम में रखा है-ऐसा व्यक्ति नैष्कर्म्य अवस्था को प्राप्त होता है। वह ज्ञानयोग के चरम परिणति रूप, क्रिया-शून्यता (परम पूर्णता) लाभ कर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
अब श्रीकृष्ण ज्ञानयोग तथा ब्रह्म के साथ एकरूपता स्थापित करने वाले गुणों का वर्णन करते हैं। विशुद्ध बुद्धि-युक्त हो कर, सांख्ययोग का सम्यक् बोध प्राप्त कर, एकान्तवास, मन को संयत रख, विषय-ज्ञान के महत्त्व की उपेक्षा कर उचित ज्ञान द्वारा इच्छाओं का अतिक्रमण कर, ध्यानयोग के निष्ठापूर्वक निरन्तर अभ्यास द्वारा अहकार को विजित कर व्यक्ति ब्राह्मी भाव अनुभव करता है। उस परम चैतन्य में नियमित एवं अविरत भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति न तो शोक से उद्विग्न होता है और न किसी प्रकार की आकांक्षा ही करता है। वह प्राणिमात्र में एक ही चैतन्य तत्त्व के दर्शन कर सबके प्रति सम भाव रखता है तथा सर्वव्यापी प्रभु की परा-भक्ति प्राप्त कर ब्रह्म में अवस्थित होता है। इस प्रकार इने-गिने व्यक्तियों द्वारा ही आचरणीय संन्यास (ज्ञानयोग) का वर्णन करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्मयोगी बन कर स्वधर्म का पालन करने को प्रबोधित करते हैं।
ईश्वर पर निर्भर रहने वाला, उनके हाथों का साधन बन कर कार्य करने वाला कर्मयोगी स्वधर्म के पालन द्वारा भगवद्-कृपा प्राप्त करता है। श्रीकृष्ण अर्जुन को फल की आकांक्षा-रहित हो स्वधर्म का पालन करने की शिक्षा देते हैं। वह उसे कर्मयोगी बन कर भगवान् के शरणागत होने को कहते हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं- "अज्ञान के कारण यद्यपि तुम स्वधर्म का पालन करने से चूक सकते हो, किन्तु प्रकृति तुम्हें वही करने के लिए उत्प्रेरित करेगी; क्योंकि कर्महीन हो कर कोई एक घड़ी के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में स्थित रह कर अपनी शक्ति द्वारा उनसे कर्म कराता है। एकमात्र भगवान् ही सब-कुछ करते हैं। अतः तुम परमात्मा की शरण ग्रहण कर स्वधर्म का पालन करो। मद्गतचित्त तथा मद्भक्त बनो। मेरे लिए यज्ञानुष्ठान करो। फिर तुम मुझमें ही लीन हो जाओगे। समस्त कर्मों के अनुष्ठान के परित्यागपूर्वक केवल मेरे शरणागत होओ। मैं तुम्हें सभी पापों से विमुक्त कर दूँगा। यह परम ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। अब तुम जैसा चाहो, वैसा करो।"
भगवान् विषय का समाहार करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य तप-रहित है तथा अहंकार के कारण जिसमें भगवान् के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं है, उसे यह रहस्यमय ज्ञान नहीं बताना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तियुक्त हो कर ईश्वर-भक्तों से यह परम गुह्य ज्ञान कहेगा, वह अवश्यमेव परमात्मा को प्राप्त होगा। जो इस संवाद का अध्ययन करेगा, वह ज्ञान-यज्ञ द्वारा ईश्वरोपासना करने वाला कहा जायेगा। जो व्यक्ति श्रीकृष्ण और अर्जुन का यह संवाद सुश्रवण करता है, वह भी शुभ लोक को प्राप्त होता है।
अन्त में श्रीकृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हारी सब शंकाएँ दूर हुईं या नहीं? अब तुम सन्देहमुक्त हुए या नहीं? अर्जुन उत्तर देते हैं कि भगवद्-कृपा से अब मेरी विगत-स्मृति मुझे है तथा युद्ध करने का साहस प्राप्त हो गया है। मेरे समस्त संशय तिरोहित हो गये हैं और अब मैं आपके उपदेशानुसार ही कार्य करूँगा।
इस प्रकार संजय ने श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस संवाद को धृतराष्ट्र को सुनाया। संजय ने व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी, जिसके परिणाम-स्वरूप उन्होंने गुह्य योग-तत्त्व का श्रवण किया था और भगवान् के विश्व-रूप का दर्शन करके आह्लादित हो गये थे।
संजय आश्वासन देते हैं कि जिस पक्ष में स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्ण तथा जिस पक्ष में धनुधारी अर्जुन होते हैं, वहाँ श्री, विजय, विभूति एवं अव्यभिचारिणी नीति निवास करती है यह निश्चय जानना चाहिए।
गीता के इस अध्याय के पाठ में मनुष्य को अपनी विकासप्रक्रम, गुणों तथा भगवान् की श्रद्धा का बोध हो जाता है। जिस भाँति जलपूरित सरिता की दिशा में अविराम गति से प्रवाहित होती रहती है, उसी भाँति आत्म विश्लेषण और विवेक-बुद्धि द्वारा अपनी संश्वलेषित पूर्ण सत्ता को ईश्वर की ओर गतिमान होना चाहिए। नदी की गति समुद्र की गतिहीन स्थिति को प्राप्त करने के लिए होती है। उसी तरह हमारे सारे प्रयास प्रयत्नरहित सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए हों।
इस प्रकार 'मोक्षसंन्यासयोग' नामक गीता का यह अन्तिम अध्याय समाप्त होता है।
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती
८ सितम्बर, १८८७ को सन्त अप्पय्य दीक्षितार तथा अन्य अनेक ख्याति-प्राप्त विद्वानों के सुप्रसिद्ध परिवार में जन्म लेने वाले श्री स्वामी शिवानन्द जी में वेदान्त के अध्ययन एवं अभ्यास के लिए समर्पित जीवन जीने की तो स्वाभाविक एवं जन्मजात प्रवृत्ति थी ही, इसके साथ-साथ सबकी सेवा करने की उत्कण्ठा तथा समस्त मानव जाति से एकत्व की भावना उनमें सहजात ही थी।
सेवा के प्रति तीव्र रुचि ने उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र की ओर उन्मुख कर दिया और जहाँ उनकी सेवा की सर्वाधिक आवश्यकता थी, उस ओर शीघ्र ही वे अभिमुख हो गये। मलाया ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। इससे पूर्व वह एक स्वास्थ्य-सम्बन्धी पत्रिका का सम्पादन कर रहे थे, जिसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर विस्तृत रूप से लिखा करते थे। उन्होंने पाया कि लोगों को सही जानकारी की अत्यधिक आवश्यकता है, अतः सही जानकारी देना उनका लक्ष्य ही बन गया।
यह एक दैवी विधान एवं मानव जाति पर भगवान् की कृपा ही थी कि देह-मन के इस चिकित्सक ने अपनी जीविका का त्याग करके, मानव की आत्मा के उपचारक होने के लिए त्यागमय जीवन को अपना लिया। १९२४ में वह ऋषिकेश में बस गये, यहाँ कठोर तपस्या की और एक महान् योगी, सन्त, मनीषी एवं जीवन्मुक्त महात्मा के रूप में उद्भासित हुए।
१९३२ में स्वामी शिवानन्द जी ने 'शिवानन्द आश्रम' की स्थापना की, १९३६ में 'द डिवाइन लाइफ सोसायटी' का जन्म हुआ; १९४८ में 'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी' का शुभारम्भ किया। लोगों को योग और वेदान्त में प्रशिक्षित करना तथा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना इनका लक्ष्य था। १९५० में स्वामी जी ने भारत और लंका का द्रुत-भ्रमण किया। १९५३ में स्वामी जी ने 'वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स' (विश्व धर्म सम्मेलन) आयोजित किया। स्वामी जी ३०० से अधिक ग्रन्थों के रचयिता हैं तथा समस्त विश्व में विभिन्न धर्मों, जातियों और मतों के लोग उनके शिष्य हैं। स्वामी जी की कृतियों का अध्ययन करना परम ज्ञान के स्रोत का पान करना है। १४ जुलाई, १९६३ को स्वामी जी महासमाधि में लीन हो गये।
A DIVINE LIFE SOCIETY PUBLICATION
HS 18 55/-