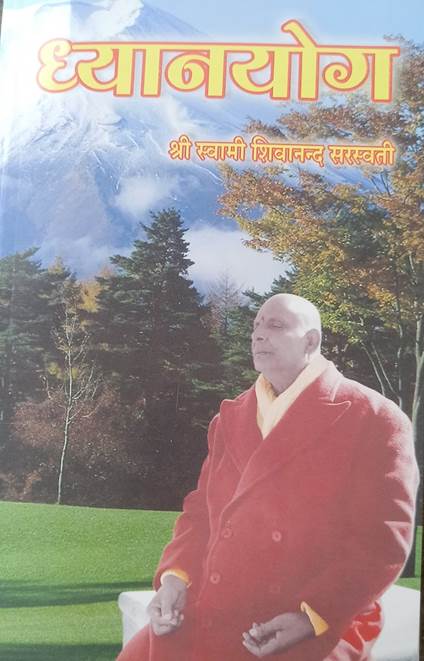
ध्यानयोग
‘DHYANA YOGA'
का हिन्दी अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी शिवानन्द
MEDITATE LOVE REALIZE SERVE THE DIVINE LIFE SOCIETY
अनुवादक
स्वामी रामराज्यम्
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर- २४९१९२
जिला : टिहरी-गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dishq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण : १९८७
द्वितीय हिन्दी संस्करण १९९६
तृतीय हिन्दी संस्करण : २००६
चतुर्थ हिन्दी संस्करण : २०१०
पंचम हिन्दी संस्करण : २०१५
षष्ठ हिन्दी संस्करण : २०१८
(१,००० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
ISBN 81-7052-064-9
HS 31
PRICE: ₹130/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर- २४९१९२, जिला टिहरी गढ़वाल, 'उत्तराखण्ड' में मुद्रित ।
For online orders and Catalogue visit: disbooks.org
प्रकाशकीय
इस पुस्तक का चतुर्थ संस्करण पाठकों के हाथों में सौंपते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। मूल अँगरेजी पुस्तक 'DHYANA YOGA' के समान यह अनुवाद भी अति लोकप्रिय रहा है। इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है इसमें उल्लिखित ध्यान-सम्बन्धी निर्देशों की व्यावहारिकता । पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने इन निर्देशों को ध्यान के व्यक्तिगत अनुभवों की कसौटी पर जाँचा-परखा है। ये निर्देश व्यावहारिक तो हैं ही, साथ ही ये ध्यानाभ्यास के सम्पूर्ण विषय-क्षेत्र को भी प्रस्तुत करते हैं।
इस पुस्तक में स्थान-स्थान पर ध्यानाभ्यास की सफलता के चरमोत्कर्ष का उल्लेख किया गया है। आशा है, सत्यान्वेषी सुधी पाठक इस चरमोत्कर्ष के बिन्दु तक पहुँचने की ललक से भर कर ध्यानाभ्यास में रत हो जायेंगे। इस पुस्तक के प्रकाशन की सार्थकता इसी में है।
- द डिवाइन लाइफ सोसायटी
अनुवादकीय
अनुवाद - कार्य में अनुवादक के मौलिक विचारों का कोई विशेष योगदान नहीं होता। वह मूल-भावों को आत्मसात् करता हुआ आगे बढ़ता है तथा यथासम्भव इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि अनुवाद मूल की ही तरह लगे।
इस दृष्टि से मेरे पास अपनी बात कहने को कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि इस असाधारण पुस्तक से सम्बद्ध रह कर जिन गहराइयों में प्रवेश करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मैं गौरवान्वित हुआ हूँ।
ध्यान के रहस्यों का उद्घाटन लेखक परम पूज्य श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने निःसंकोच हो कर किया है। इस कारण ध्यान के जो रहस्य कन्दराओं की कारा में बन्द रहते, वे परम तत्त्व के अन्वेषी साधकों की झोली में आ पड़े हैं।
प्रवाह की दृष्टि से कहीं-कहीं विचारों का क्रम परिवर्तित कर दिया गया है। मूल पुस्तक की पुनरावृत्तियों को ज्यों-का-त्यों रखा गया है; क्योंकि वे मुख्य-मुख्य विचारों पर जोर देने में सहायक सिद्ध हुई हैं।
अँगरेजी ग्रन्थ के मूल भावों का अवगाहन करते समय मैं चिन्तन-मनन के जिन स्तरों पर पहुँचा हूँ, उन स्तरों पर पाठक पहुँच कर मेरी तरह अनुभूति कर सकें—यह मेरा प्रयास आद्योपान्त रहा है।
- अनुवादक
भूमिका
तैल-धारा के सतत प्रवाह के सदृश किसी एक ही विचार के प्रवाह को बनाये रखना ही ध्यान है। ध्यान दो प्रकार का होता है—मूर्त और अमूर्त। किसी चित्र या मूर्त पदार्थ पर ध्यान करना मूर्त ध्यान है। किसी अमूर्त विचार या धैर्य-जैसे किसी गुण पर ध्यान करना अमूर्त ध्यान है। प्रारम्भ में साधक को मूर्त ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। कुछ साधकों के लिए मूर्त ध्यान की अपेक्षा अमूर्त ध्यान करना अधिक सरल होता है।
साधकों को प्रत्याहार और धारणा में सुस्थित होने के बाद ही ध्यान का प्रारम्भ करना चाहिए। यदि इन्द्रियाँ उछल-कूद मचा रही हों, मन किसी बिन्दु पर टिक नहीं पा रहा हो, तो दीर्घ काल तक अभ्यास करने पर भी सफलतापूर्वक ध्यान नहीं किया जा सकता। साधना-पथ पर क्रम से धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ध्येय पर मन को टिकाने का प्रयास करते हुए उसे (मन को) बार-बार भटकने से रोकना चाहिए। भटकने की इसकी प्रकृति पर नियन्त्रण प्राप्त करना आवश्यक है। मन 'अनावश्यक कामनाओं को हटा देना चाहिए। कामना-रहित व्यक्ति ही शान्त हो कर ध्यान का अभ्यास कर सकता है। ध्यान के अभ्यास की दो महत्त्वपूर्ण पूर्वापेक्षाएँ हैं—सात्त्विक हलका आहार तथा ब्रह्मचर्य पालन ।
चेतना दो प्रकार की होती है—संकेन्द्रित चेतना तथा औपान्तिक (marginal) चेतना । जब आप त्रिकुटी पर ध्यान करते हैं, उस समय संकेन्द्रित चेतना क्रियाशील रहती है। ध्यान करते समय शरीर पर बैठी हुई मक्खी को जब आप हाथ उठा कर भगाते हैं, तब उस समय मक्खी के प्रति आपकी सजगता औपान्तिक चेतना है। क्षण मात्र के लिए भी अग्नि के सम्पर्क में आया हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता, भले ही उसे उर्वरा भूमि में बो दिया जाये। इसी प्रकार कुछ देर के लिए ध्यान में रत जो मन अस्थिर होने के कारण ऐन्द्रिय पदार्थों की तरफ दौड़ने लगता है, उससे योग-साधना में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।
प्रारम्भिक अभ्यासियों को प्रतिदिन वेदान्त के कुछ महत्त्वपूर्ण कथनों का स्मरण करना चाहिए। प्रवाहित होने वाली विचार-तरंग को प्रोत्साहित करें। तब मन चोर की तरह लुकता - छिपता फिरेगा और अन्त में काबू में आ जायेगा।
योगवासिष्ठ के अनुसार, “नये अभ्यासी के लिए उचित होगा कि वह अपने मन के आधे भाग को सुख-भोग के पदार्थों से, एक चौथाई भाग को दर्शनशास्त्र तथा शेष एव चौथाई भाग को गुरु-भक्ति से परिपूर्ण कर ले। जब कुछ अभ्यास हो जाये तब आधे भाग को गुरु भक्ति से, एक चौथाई भाग को सुख भोग के पदार्थों से तथा शेष भाग क दर्शनशास्त्र के अर्थ-बोध से भर लेना चाहिए। साधना में निपुणता प्राप्त करने के पश्चात उसे प्रतिदिन अपने मन के आधे भाग को दर्शनशास्त्र के ज्ञान तथा परम त्याग से और शेष आधे भाग को ध्यान तथा गुरु-भक्ति से परिपूरित कर लेना चाहिए।” अन्ततः आप प्रतिक्षण ध्यान में रहने की स्थिति में पहुँच जायेंगे। सच्चिदानन्द ब्रह्म का सतत ध्यान करें तथा जीते-जी परम निष्कल्मष पद प्राप्त कर लें।
विश्व-प्रार्थना
हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव !
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है।
तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ हो।
तुम सच्चिदानन्दघन हो ।
तुम सबके अन्तर्वासी हो ।
हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समत्व प्रदान करो।
श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो ।
हमें आध्यात्मिक अन्तःशक्ति का वर दो,
जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों।
हम अहंकार, काम, लोभ, घृणा, क्रोध और द्वेष से रहित हों।
हमारा हृदय दिव्य गुणों से परिपूरित करो।
हम सब नाम-रूपों में तुम्हारा दर्शन करें।
तुम्हारी अर्चना के ही रूप में इन नाम-रूपों की सेवा करें।
सदा तुम्हारा ही स्मरण करें।
सदा तुम्हारी ही महिमा का गान करें।
तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे अधर-पुट पर हो।
सदा हम तुममें ही निवास करें।
-स्वामी शिवानन्द
परिचायक निबन्ध
ध्यान का विज्ञान
एकाग्रता का अर्थ है मन को किसी विशेष पदार्थ पर टिकाना। उस पदार्थ के ज्ञान का निर्बाध प्रवाह ध्यान है। दूसरे शब्दों में, एकाग्रता के विषय के नियमित चिन्तन-प्रवाह को ध्यान कहते हैं। एकाग्रता के बाद ध्यान की स्थिति आती है। एकाग्रता ध्यान में विलय हो जाती है। ध्यान से मन के द्वार खुलते हैं और तब अन्तर्प्रज्ञा तथा अन्य अनेक क्षमताएँ प्रकाश में आती हैं। ध्यान से किसी भी वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान की स्थिति में सांसारिक विचार खो जाते हैं। अष्टांगयोग के अन्तर्गत योग का सप्तम अंग ध्यान है।
ध्यान तथा अन्य आध्यात्मिक विधियों के अभ्यास के लिए एक अलग कक्ष होना चाहिए। उसे भगवान् का मन्दिर ही मानें। किसी को उस कक्ष में न जानें दें। पवित्रता और श्रद्धा से परिपूर्ण मन से कमरे में प्रवेश करें। ईर्ष्या, कामुकता, लोभ तथा क्रोध के विचारों को कक्ष की चहारदीवारी के अन्दर फटकने न दें। सांसारिक विषयों पर चिन्तन या बातचीत न करें। कारण यह है कि कोई भी शब्द जो बोला जाता है, कोई भी विचार जो मन में आता है, कोई भी कार्य जो किया जाता है, वह नष्ट नहीं होता। वह कक्ष के चारों ओर के आकाश के सूक्ष्म संस्तरों पर प्रतिबिम्बित होता है और निश्चित रूप से मन को प्रभावित करता है।
ध्यान के कक्ष को महान् सन्तों, पैगम्बरों तथा सद्गुरुओं के प्रेरक चित्रों से सुसज्जित करें। कक्ष में किसी प्रमुख स्थान पर अपने इष्टदेवता-ईसामसीह, कृष्ण, शंकर, देवी आदि का चित्र रखें। यह चित्र पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। इष्टदेवता के सामने अपना आसन बिछा लें। हाथ, पैर, मुँह आदि धो लेने के पश्चात् ही कक्ष में प्रवेश करें। प्रवेश करने के तुरन्त बाद कर्पूर या सुगन्धित अगरबत्ती जलायें। इष्टदेवता के सम्मुख आसन पर बैठ जायें। अपने निकट ही भगवद्गीता, उपनिषद्, वेदान्तसूत्र, रामायण-जैसे सद्ग्रन्थ रख लें। भगवन्नाम का उच्चारण करें या भजन गायें। इसके बाद एकाग्रता या ध्यान का अभ्यास करें।
ध्यान के लिए प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्थान ढूँढ पाना कठिन है। हर स्थान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। अतः दूसरे स्थानों की तुलना में जो स्थान आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे, उसी का चयन कर लें। एक बार स्थान का चयन करने के बाद उसे दोबारा कभी न बदलें। कठिनाई उपस्थित होने पर भी न बदलें। कठिनाइयों का सामना करें। भारत में ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बदरीनारायण, गंगोत्तरी, वृन्दावन, वाराणसी, नासिक तथा अयोध्या ध्यान के लिए सर्वोत्तम स्थान हैं।
ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय निःसन्देह ब्राह्ममुहूर्त (प्रातः काल चार से छह बजे के बीच का समय है)। यह वह समय होता है जब नींद पूरी हो जाने के बाद मन बिलकुल शान्त हो जाता है तथा अपेक्षाकृत अधिक पवित्र रहता है। उस समय यह कोरे कागज की तरह होता है। इसी तरह के मन को मनचाहे ढंग से बदला जा सकता है। इस समय वातावरण भी शुद्ध और सात्त्विक रहता है।
प्रारम्भ में आप दो बार ध्यान कर सकते हैं—प्रातः ४ से ५ बजे तक तथा सायंकाल ७ से ८ बजे तक। जैसे-जैसे अभ्यास होता जाये, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आप अभ्यास करने की अवधि धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। साथ ही दिन में तीसरी बार भी (पूर्वाह्न १० या ११ बजे के बीच) ध्यान के लिए बैठ सकते हैं।
किसी सुविधाजनक आसन में ध्यान के लिए बैठ जायें। शिर, गरदन और धड़ को सीधा रखें। आँखें बन्द कर लें। अब नासिकाग्र, भ्रूमध्य-बिन्दु, हृदय-कमल या शिर के सबसे ऊपरी भाग पर मन को एकाग्र करें। एकाग्रता-बिन्दुओं पर अभ्यास करने के बाद जिस एक बिन्दु पर मन को एकाग्र करना सर्वाधिक अनुकूल लगे, उसका चयन कर लें। मान लें कि आपने हृदय-कमल के एकाग्रता-बिन्दु का चयन किया है। अब आपको हृदय-कमल के अतिरिक्त अन्य किसी एकाग्रता - बिन्दु की बात नहीं सोचनी चाहिए । जब ऐसा होगा, तभी आध्यात्मिक विकास की गति तेज होगी।
ध्यान दो प्रकार का होता है—सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। कृष्ण, शिव, भगवान् राम, ईसामसीह आदि का ध्यान करना सगुण ध्यान है। यह ईश्वर का उसके गुणों तथा रूप-सहित ध्यान करना है। सगुण ध्यान करते समय सम्बन्धित ईश्वर के नाम का जप भी किया जाता है। आत्म-तत्त्व पर ध्यान निर्गुण ध्यान कहलाता है। वेदान्ती साधक निर्गुण ध्यान करते हैं। 'ॐ', 'सोऽहम्', 'शिवोऽहम्', 'अहं ब्रह्मास्मि' और 'तत् त्वम् असि' पर ध्यान करना निर्गुण ध्यान है।
दहकती हुई अग्नि में लोहे की एक शलाका डाल दें। थोड़ी देर में लोहा आग की तरह लाल हो जायेगा। अब इसे आग से निकाल लें। थोड़ी देर में लाल रंग विलीन हो जायेगा। यदि आप चाहें कि इसका लाल रंग बना रहे, तब इसे सदैव आग में ही रखना होगा। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि मन ब्रह्मज्ञान की अग्नि से आवेशित रहे, तो इसे अनवरत और गहन ध्यान की सहायता से इस अग्नि के सम्पर्क में रखना होगा। दूसरे शब्दों में आपको ब्रह्म-चेतना का प्रवाह सतत बनाये रखना होगा।
ध्यान सर्वाधिक प्रभावोत्पादक मानसिक तथा तन्त्रिका प्रभावी टानिक है। ध्यान की पवित्र स्फुरणाएँ शरीर की प्रत्येक कोशिका में व्याप्त उन विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाती हैं, जो मानव शरीर को विरासत में मिले हैं। जो साधक नियमित रूप से ध्यान करते हैं, उन्हें दवाओं पर धन खर्च नहीं करना पड़ता। ध्यान करते समय जो शक्तिशाली शामक तरंगें उत्पन्न होती हैं, वे मन, स्नायुओं, कोशिकाओं और विभिन्न अंगों पर बहुत अनुकूल प्रभाव डालती हैं। ईश्वर के चरण-कमलों से दैवी ऊर्जा तैलधारा-सदृश प्रवाहित हो कर ध्यान के अभ्यासी तक पहुँचने लगती है।
यदि आप आधा घण्टे तक ध्यान करें, तो इसके प्रभाव से प्राप्त शान्ति और आध्यात्मिक शक्ति से आप एक सप्ताह तक अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से जूझ सकेंगे। ऐसा हितकारी प्रभाव होता है ध्यान का! दैनिक जीवन में आप विचित्र स्वभावों वाले तरह-तरह के लोगों के सम्पर्क में आते हैं। उनके साथ निर्वाह करने हेतु आप ध्यान के द्वारा अपेक्षित शक्ति और शान्ति प्राप्त करें तथा सब प्रकार की चिन्ताओं से जायें । मुक्त हो
बुद्धिमान् व्यक्ति सतत ध्यान की तेज धार वाली तलवार से अहं की ग्रन्थि काट डालते हैं। इसके बाद वे आत्मज्ञान, आत्म-साक्षात्कार या पूर्ण बोध को प्राप्त करते हैं। उनके कर्म-बन्धन कट जाते हैं। अतः सतत ध्यानमग्न रहें। परमानन्द प्राप्त करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। साधना के प्रारम्भ में लक्ष्य से मन इधर-उधर भागेगा और इस कारण निराशा हो सकती है। थकान भी महसूस हो सकती है। बाद में मन एक बिन्दु पर टिकने लगेगा। तब आप परमानन्द के सागर में समा जायेंगे।
नियमित ध्यान करने से अन्तर्प्रज्ञा का उदय होता है तथा मन शान्त और स्थिर हो जाता है। भाव-विभोर हो कर आह्लादित मन से साधक परम पुरुष के सम्पर्क में आता है। ध्यानयोग के मार्ग पर नियमित चलने से सभी प्रकार के भ्रम और सन्देह स्वयं समाप्त हो जाते हैं। फिर योग-निसेनी के अगले डण्डे पर पैर रखने के रास्ते की जानकारी आपको सहज ही मिलने लगती है। एक रहस्यमय आन्तरिक वाणी आपका मार्ग-निर्देशन करने लगती है। साधक गण! आप इस वाणी को ध्यानपूर्वक सुनें।
जब आपको आध्यात्मिक बोध की दमक दिखायी पड़े, भयभीत न हो जायें। यह असीम आनन्द का एक नया अनुभव होगा। पीछे नहीं लौटें। ध्यान का अभ्यास करना बन्द न करें। अभी तो सत्य की एक झलक मात्र देखने को मिली है। यह चरम सत्य थोड़े ही है। अभी तो आप एक नये आधार-स्थल पर खड़े हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करें और सभी प्रलोभनों का संवरण करते हुए भूमा (असीम) के लक्ष्य तक पहुँच जायें। तब आप अनश्वरता के अमृत का पान करेंगे। यही चरमावस्था है। अब आप शाश्वत विश्राम की स्थिति में होंगे। अब आपको और अधिक ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यही आपका चरम लक्ष्य है।
आपके अन्दर अनन्त प्रसुप्त शक्तियाँ और अव्यक्त क्षमताएँ हैं। इसका ज्ञान आपको नहीं है। ध्यान के अभ्यास द्वारा इन प्रसुप्त शक्तियों-क्षमताओं को जाग्रत करें। आप अपनी इच्छा-शक्ति को विकसित करें तथा मन और इन्द्रियों को अपने नियन्त्रण में रखें। अपने को शुद्ध रखते हुए ध्यान का नियमित अभ्यास करें। तभी आप महामानव या ईश- मानव बन सकेंगे।
सिद्धि की तरह की कोई वस्तु नहीं हुआ करती। साधारण व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक तथ्यों से अपरिचित रहता है। वह विस्मृति में ही डूबा रहता है। उच्च अनुभवातीत ज्ञान के द्वार उसके लिए बन्द रहते हैं। इसीलिए वह किसी भी असाधारण घटना को सिद्धि समझने लगता है। परन्तु योगी, जो योग के आलोक में सब-कुछ देख-समझ चुका होता है, सिद्धियों के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता। गाँव वाला पहली बार हवाई जहाज देखता है, तब आश्चर्य में डूब जाता है। उसी प्रकार सांसारिक व्यक्ति जब पहली बार कोई असाधारण दृश्य देखता है, तब हक्का-बक्का रह जाता है।
प्रत्येक मानव में विभिन्न प्रकार की क्षमताएँ निहित हैं। वह ज्ञान और शक्ति का बारूदखाना है। जैसे-जैसे उसका क्रम विकास होता जाता है, उसकी शक्तियाँ, क्षमताएँ और गुण प्रकट होते जाते हैं। अब वह अपने वातावरण को परिवर्तित कर सकता है तथा दूसरों को प्रभावित कर सकता है। वह दूसरों के मन को अपने वश में कर सकता है। वह बाह्य तथा आन्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह अति-चेतना की स्थिति में पहुँच सकता है। कल्पना करें कि किसी अँधेरे कमरे में किसी पात्र के अन्दर जलता हुआ एक दीपक रखा हुआ है। यदि वह पात्र टूट जाये (अर्थात् अविद्या का नाश हो जाये तथा परिणाम-स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य समाप्त हो जाये; आप शरीर की चेतना से ऊपर उठ जायें), तो आपको हर स्थान पर आत्मा का परम प्रकाश दृष्टिगोचर होने लगेगा।
यदि पानी से भरा हुआ घड़ा नदी के अन्दर हो और घड़ा फूट जाये, तो क्या होगा ? घड़े का पानी और नदी का पानी एक हो जायेगा। उसी प्रकार आत्मा का ध्यान करने से शरीर का घड़ा फूट जाता है। तब जीवात्मा परमात्मा से मिल कर एक हो जाता है।
जिस प्रकार लालटेन के अन्दर प्रकाश होता रहता उसी प्रकार आपके हृदय-दीप में भी अनन्त काल से दिव्य प्रकाश हो रहा है। आँखें बन्द करें। इस दिव्य प्रकाश में विलीन हो जायें। हृदय की गहराइयों में उतर कर दिव्य प्रकाश पर मन को एकाग्र करें और फिर ईश्वर की अग्नि-शिखा के साथ एकाकार हो जायें।
यदि दीप की बत्ती छोटी हो, तो रोशनी भी कम होगी। बत्ती बड़ी होगी, तो प्रकाश भी प्रखर होगा। उसी प्रकार यदि जीव (जीवात्मा) शुद्ध है और यदि उसके द्वारा ध्यान का अभ्यास किया जा रहा है, तो आत्मा की अभिव्यक्ति बड़ी सशक्त होगी। उसमें से एक प्रखर प्रकाश का विकिरण होगा। यदि जीव अशुद्ध और अपुनरुज्जीवित (unregenerate) है, तो वह जले हुए कोयले की तरह बन कर रह जायेगा। दिये की बत्ती जितनी बड़ी होती है, उतना ही अधिक प्रकाश होता है, इसी प्रकार जीव जितना अधिक शुद्ध होगा, उतनी ही उसकी अभिव्यक्ति सशक्त होगी।
चुम्बक यदि शक्तिशाली होगा, तो वह दूर रखे हुए लोहे को भी आकर्षित कर लेगा। उसी प्रकार यदि योगी उच्च कोटि का साधक है, तो सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों पर अधिक प्रभाव डालेगा। वह सुदूर स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों पर भी अपना अधिक प्रभाव डालेगा।
ध्यान की अग्नि में सारे अवगुण जल कर नष्ट हो जाते हैं। तब एकाएक आत्मज्ञान (दिव्य प्रज्ञा) प्रकट होता है। इससे मुक्ति का द्वार खुलता है।
ध्यान करते समय इस बात के प्रति सजग रहें कि आप कितनी अवधि तक सांसारिक चिन्तन से मुक्त रह पाते हैं। अपने मन पर कड़ी निगाह रखें। यदि यह अवधि बीस मिनट है, तो इसे बढ़ाने का प्रयत्न करें। बार-बार मन को ब्रह्म के चिन्तन से परिपूरित करें।
ध्यान करते समय आँखों पर जोर न डालें। मन के साथ लड़ाई भी न करें। तनावमुक्त हो कर ध्यान करें। दिव्य विचारों को सहज रूप से प्रवाहित होने दें। अपने लक्ष्य (ध्यान के एकाग्रता - बिन्दु) के बारे में स्थिरता और गम्भीरता से विचार करें। अनपेक्षित विचारों को जबरदस्ती न भगायें। मन में उदात, सात्त्विक विचारों को आने दें। बुरे विचार स्वतः ही चले जायेंगे।
यदि ध्यान करते समय मन पर बहुत जोर पड़ता हो, तो थोड़े दिनों के लिए ध्यान करने का समय प्रत्येक बैठक में कम कर दें। बहुत गहन ध्यान न करें। सामान्य स्थिति वापस आ जाने पर ध्यान करने का समय दोबारा बढ़ा दें। पूरे साधना-काल में अपनी सहज बुद्धि का उपयोग करते रहें। मैं हमेशा निम्नांकित बात पर जोर देता हूँ :
"एक सहस्र वर्ष तक एक पैर पर खड़े हो कर किया जाने वाला तप ध्यानयोग के सोलहवें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकता" (पैंगल उपनिषद्) ।
जो साधक चार-पाँच घण्टों तक लगातार ध्यान करते हैं, वे पैर थक जाने पर बीच में ध्यान का आसन एक बार बदल सकते हैं। कभी-कभी पैरों या जाँघों के किसी भाग में रक्त एकत्रित हो जाता है और कष्ट देने लगता है। दो घण्टे के बाद आप आसन बदल दें या पैरों को पूरा फैला कर किसी दीवाल या तकिये का सहारा ले लें। मेरुदण्ड सीधा रखें। यह एक सुविधाजनक आसन है। एक दूसरा उपाय यह है कि दो कुरसियाँ पास-पास रख लें। एक कुरसी पर बैठें और दूसरी कुरसी पर पैर फैला कर रखें।
प्रतिदिन वैराग्य, ध्यान और सात्त्विक गुणों (धैर्य, दृढ़ता, करुणा, प्रेम, क्षमा आदि) में वृद्धि करें। वैराग्य और ये गुण ध्यान के अभ्यास में सहायक सिद्ध होते हैं। ध्यान से सात्त्विक गुणों में वृद्धि होती है।
ध्यान करने से मन-मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणाली में परिवर्तन आता है। नयी स्नायु- धाराएँ, नवीन प्रदोलन (vibrations), नयी कोशिकाएँ तथा नये मार्ग निर्मित होने लगते हैं। मन और स्नायु प्रणाली का नये सिरे से प्रत्यारोपण हो जाता है। नया मन, नया हृदय, नयी अनुभूतियाँ, नयी भावनाएँ, नयी चिन्तन-प्रणाली, नयी कार्य-प्रणाली तथा दूसरों के प्रति नयी दृष्टि (सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति हैं)—ये हैं ध्यान के सुखद परिणाम |
ध्यान करते समय भाव-समाधि या हर्षोन्माद की स्थिति आ सकती है। यह स्थिति पाँच प्रकार की होती है— अल्पमात्रिक, क्षणिक, आप्लावनकारी, वाहक तथा सर्वव्यापी । अल्पमात्रिक स्थिति रोमांच या रोमहर्षण की स्थिति होती है। इसमें त्वचा हंस 1 की त्वचा के समान हो जाती है। क्षणिक स्थिति क्षण-क्षण में कौंधने वाली बिजली के समान है। आप्लावनकारी स्थिति लहरों के समान है जो लगातार तट पर टकराती रहती है। शरीर रूपी तट पर हर्षोन्माद की लहरें अवतरित होती हैं और टकराती हैं। यह स्थिति बड़ी बलवती होती है। यह शरीर को धरती' उठा कर हवा में छोड़ देती है। सर्वव्यापी स्थिति में शरीर सम्पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है और फूले हुए गुब्बारे की तरह उड़ने लगता है।
"योगी साधक को चाहिए कि उसे जो कुछ भी दिखायी पड़े, उसे वह आत्मा ही माने। अपने कानों से सुनायी पड़ने वाला शब्द, अपनी नाक से सूँघी जाने वाली गन्ध, अपनी जिह्वा से मिलने वाला रस तथा अपनी त्वचा से मिलने वाली स्पर्शानुभूति – ये सब उसकी दृष्टि में आत्मा के ही स्वरूप होने चाहिए। इस प्रकार योगी को प्रयत्न करके प्रतिदिन एक याम (अर्थात् तीन घण्टे तक अपनी ज्ञानेन्द्रियों को सन्तुष्ट करना चाहिए। तब योगी साधक को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यथा— अतीन्द्रिय दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण, क्षण-भर में ही अपने को सुदूर क्षेत्रों में ले जाने की क्षमता, मनचाहा रूप धारण करने की क्षमता, वाक्-शक्ति, अन्तर्धान हो जाने की क्षमता तथा लोहे से सोना बना देने की क्षमता” (योगतत्त्वोपनिषद्) ।
एक निपुण धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते समय इस तथ्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहता है कि उसके पैर एक विशेष स्थिति में रहेंगे। वह एक विशेष प्रकार से तीर-कमान पकड़ता है। वह यह भी जानता है कि लक्ष्य-भेद में सफलता प्राप्त करने के लिए ये बातें अति-आवश्यक हैं। उसी प्रकार साधक भी इसके प्रति जागरूक रहता है कि ध्यान और समाधि की स्थिति में पहुँचने हेतु उसे विशेष प्रकार का भोजन करना होगा, विशेष प्रकार के लोगों की संगति में रहना होगा, विशेष प्रकार के वातावरण में रहना होगा तथा विशेष प्रकार की जीवन-पद्धति का अनुसरण करना होगा।
जिस प्रकार एक समझदार रसोइया अपने स्वामी की भोजन सम्बन्धी रुचि का ध्यान रखते हुए तदनुकूल भोजन तैयार करता है और स्वामी के अनुग्रह का लाभ प्राप्त करता है, उसी प्रकार साधक भी ध्यान और समाधि के लिए आवश्यक परिस्थितियों (जैसे पोषण आदि) के प्रति जागरूक रहता है और उनके अनुकूल आचरण करके बार- बार हर्षोन्माद का लाभ प्राप्त करता है।
ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करना ही पर्याप्त नहीं है; मन की एकाग्रता भी अत्यावश्यक है। सदाचारपूर्ण जीवन ध्यान और एकाग्रता का उपयुक्त उपकरण बनने के लिए मन को मात्र तैयार करता है। एकाग्रता और ध्यान ही अन्ततः साधक को आत्म-साक्षात्कार या ब्रह्म-साक्षात्कार के लक्ष्य तक पहुँचाते हैं।
"योगी को भय, क्रोध, आलस्य, अति-निद्रा, अति जागरण, अति भोजन तथा अति-उपवास से बचना चाहिए। यदि वह प्रतिदिन इन नियमों का पालन करे, तो निःसन्देह तीन महीने की अवधि में उसमें आध्यात्मिक प्रज्ञा का उदय होगा, चार महीने में वह देव-दर्शन करने लगेगा, पाँच महीने के अन्दर वह ब्रह्मनिष्ठ बन जायेगा और छह महीने की अवधि में वह सचमुच कैवल्य की स्थिति प्राप्त कर लेगा" (अमृतनाद उपनिषद्) ।
ध्यान की स्थिति में कभी-कभी कुछ दृश्य दिखायी पड़ते हैं। इनमें कुछ दृश्य मात्र आपके विचार के मूर्त रूप ही होते हैं, तथा कुछ वास्तविक (दिव्य) दृश्य होते हैं। ध्यान करते समय मस्तिष्क में नये आध्यात्मिक खाँचे निर्मित होते हैं और उन्हीं खाँचों के मार्ग से मन की ऊर्ध्वगामी यात्रा प्रारम्भ होती है। एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास करते समय मन को विविध ढंगों से प्रशिक्षित करना होगा। तभी स्थूल मन सूक्ष्म मन में रूपान्तरित हो जायेगा ।
ध्यान के अभ्यास के प्रारम्भिक चरण में मस्तक में लाल, सफेद, नीला, हरा तथा लाल-हरा मिश्रित रंग दिखायी पड़ते हैं। ये पंचतत्त्वों के प्रकाश हैं। प्रत्येक तत्त्व के लिए एक विशिष्ट रंग निर्धारित रहता है। पृथ्वी तत्त्व के लिए पीला, जल-तत्त्व के लिए सफेद, अग्नि-तत्त्व के लिए लाल, वायु-तत्त्व के लिए हरा तथा आकाश-तत्त्व के लिए नीला रंग है। इसलिए ध्यान में ये रंग पंचतत्त्वों के कारण ही दिखलायी पड़ते हैं।
ध्यान करते समय कभी-कभी मस्तक के सामने बड़े आकार का चमकता हुआ सूर्य, चन्द्रमा या बिजली दिखायी पड़ती है। इन पर ध्यान न दें। इनके आकर्षण से बचें। इनके मूल स्रोतों के सम्पर्क में आने के लिए ध्यान की गहराई में जायें।
कभी-कभी ध्यान में देवताओं, नित्य-सिद्धों और अमर पुरुषों के दर्शन होते हैं। उन्हें समुचित आदर देते हुए उनका स्वागत करें। उनके सामने नमन करें। उनसे सत्परामर्श प्राप्त करें। उनसे भय न रखें। वे आपको प्रोत्साहन देने तथा आध्यात्मिक सहायता करने के लिए ही प्रकट होते हैं।
"अपने शरीर को नीचे की अरणि तथा प्राण को ऊपर की अरणि बना कर ध्यानाभ्यास-रूपी मन्थन-क्रिया के द्वारा काष्ठ में व्याप्त हुई अग्नि की भाँति सबके भीतर व्याप्त परमात्मा का साक्षात्कार करें" (ध्यानबिन्दु उपनिषद्) ।
साधकों की सुविधा के लिए नीचे ध्यान के कुछ अभ्यास दिये जा रहे हैं:
(१)
अपने सामने भगवान् ईसामसीह का चित्र रखें। ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठें। चित्र को टकटकी लगा कर तब तक देखें, जब तक आँखों से आँसू न गिरने लगें। क्रास, उनके वक्ष, लम्बे बालों, सुन्दर दिखने वाली दाढ़ी, गोल-गोल आँखों, शरीर के विभिन्न अंगों और आध्यात्मिक प्रभा मण्डल पर अपना ध्यान (एक-एक करके) ले जायें। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न सद्गुणों-प्रेम, उदारता, करुणा तथा सहिष्णुता का चिन्तन करें। उनके जीवन के विभिन्न रोचक पक्षों, उनके चमत्कारों तथा उनकी असामान्य शक्तियों के बारे में सोचें। अब आँखें बन्द कर लें और चित्र का मानस-दर्शन करें। इस अभ्यास को बार-बार दोहरायें।
(२)
भगवान् हरि का चित्र अपने सामने रखें। ध्यान के किसी आसन में बैठें। चित्र पर तब तक त्राटक का अभ्यास करें, जब तक आँसू न गिरने लगें। फिर उनके चरण-कमलों, पैरों, पीले रेशमी वस्त्रों, वक्ष पर पड़े हुए हीरक जटित सोने के हार, कौस्तुभ मणि, कर्ण-फूलों, चेहरे, मुकुट, ऊपरी दाहिने हाथ के चक्र, ऊपरी बायें हाथ के शंख, निचले दाहिने हाथ की गदा तथा निचले बायें हाथ के कमल के फूल पर एक-एक करके ध्यान ले जायें । आँखें बन्द करके चित्र का मानस-दर्शन करें। इस अभ्यास को कई बार दोहरायें।
(३)
हाथों में वंशी लिये हुए भगवान् कृष्ण का चित्र अपने सामने रखें। ध्यान के किसी आसन में बैठें। तब तक उस चित्र को अपलक निहारते रहें, जब तक आँखों से आँसू न आने लगें। नूपुरों से सुसज्जित उनके चरणों, उनके पीत वस्त्रों, गले के आभूषणों, कौस्तुभ मणि के हार, रंग-बिरंगे फूलों से बनी लम्बी माला, कर्ण-कुण्डलों, बहुमूल्य रत्नों वाले मुकुट, लम्बे, घने काले बालों, चमकती आँखों, माथे पर लगे हुए तिलक, आकर्षक प्रभा मण्डल, बाजूबन्दों, कंगनों से सुसज्जित हाथों और वंशी के बारे में सोचें। अब आँखें बन्द करके चित्र का मानस-दर्शन करें। इस क्रिया को कई बार दोहरायें।
(४)
प्रारम्भिक साधकों के लिए यह ध्यान की एक विधि है। अपने ध्यान कक्ष में वज्रासन लगा कर बैठें। आँखें बन्द कर लें। सूर्य की चमक का ध्यान करें। चन्द्रमा की दीप्ति या तारों की द्युति का ध्यान करें।
(५)
समुद्र की उदारता और असीमता का चिन्तन करें। तब समुद्र की असीम ब्रह्म से तुलना करें। समुद्र की लहरों, फेनों तथा हिमशैलों की भी तुलना ब्रह्म के अनेकानेक नामों से करें। समुद्र के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करें। शान्त हो जायें। समुद्र की तरह अपना विस्तार करें।
(६)
यह एक दूसरे प्रकार का ध्यान है। हिमालय का ध्यान करें। गंगोत्तरी के हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती हुई; ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी आदि मुख्य शहरों से प्रवाहित होती हुई तथा अन्त में गंगासागर के निकट बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हुई गंगा का ध्यान करें। हिमालय, गंगा और सागर—केवल इन तीन का ही चिन्तन करें। पहले गंगोत्तरी के बरफानी स्थानों पर; फिर गंगा और फिर सागर में मन को टिकायें। १० मिनट तक मन को क्रम से इसी तरह घुमाते रहें।
(७)
इस जगत् के नामों और रूपों में एक सर्वव्यापक शक्ति निहित है। इस निराकार शक्ति का ध्यान करें। अन्ततः वह ध्यान परम (Absolute), निर्गुण, निराकार चेतना के साक्षात्कार के रूप में फलीभूत होगा।
(८)
पद्मासन में बैठें। नेत्र बन्द कर लें। केवल निराकार वायु का ध्यान करें। वायु पर ही मन को एकाग्र करें। इसके सर्वव्यापक रूप का चिन्तन करें। इससे एकमात्र जीवन्त सत्य - नाम-रूप-रहित ब्रह्म का—साक्षात्कार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
(९)
ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जायें। नेत्र बन्द कर लें। नामों और रूपों में सन्निहित करोड़ों सूर्यों की आभा के समान परम और असीम दीप्ति का चिन्तन करें। यह निर्गुण ध्यान का एक दूसरा प्रकार है।
(१०)
विस्तृत और नीले आकाश पर मन को एकाग्र करके उसका ध्यान करें। यह भी निर्गुण ध्यान है। पूर्व-वर्णित ध्यान-विधियों से मन ससीम रूपों का चिन्तन करना बन्द कर देगा। जैसे-जैसे इसकी विषय-सामग्री इससे छूटती जायेगी, वह शान्ति के सागर में विलीन होता जायेगा। तब वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जायेगा ।
(११)
अपने सामने 'ॐ' का चित्र रखें। खुली आँखों से तब तक एकटक देखें, जब तक कि आँखों से आँसू न गिरने लगे। 'ॐ' का चिन्तन करें। इस चिन्तन के साथ शाश्वतत्व, असीमता तथा अमरता के विचारों को सम्बद्ध करें। सोचें कि मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, कोयल के गीत, संगीत के सातों स्वर-सभी 'ॐ' से निःसृत हुए हैं। 'ॐ' वेदों का सार है। कल्पना करें कि 'ॐ' धनुष है, मन तीर है और ब्रह्म (ईश्वर) लक्ष्य है। बहुत सावधानी से लक्ष्य-भेद करें। जिस प्रकार अन्त में तीर और लक्ष्य एक हो जाते हैं, इसी प्रकार आप और ब्रह्म भी एक हो जायेंगे। 'ॐ' का अनुदात्त स्वराघात (accent) सभी पापों को भस्म कर देता है और उदात्त स्वराघात सभी सिद्धियाँ प्रदान करता है। जो साधक इस 'ॐ' का उच्चारण तथा ध्यान करता है, वह संसार के सभी धर्मग्रन्थों का ध्यान करता है।
(१२)
अपने ध्यान कक्ष में पद्मासन या सिद्धासन लगा कर बैठ जायें। अपनी श्वास के प्रवाह के प्रति जागरूक हो जायें। आपको 'सोऽहम्' की ध्वनि सुनायी पड़ेगी। श्वास लेते समय 'सो' की ध्वनि और श्वास छोड़ते समय 'ह' की ध्वनि । 'सोऽहम्' का अर्थ है—मैं वह हूँ। आपकी श्वास परमात्मा के साथ आपकी अभिन्नता का स्मरण दिला रही है। आप प्रति मिनट १५ बार 'सोऽहम्' का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार आप अनजाने में ही प्रतिदिन २१, ६०० बार 'सोऽहम्' का उच्चारण करते हैं। सत्ता, ज्ञान, परमानन्द, परम तत्त्व, पवित्रता, शान्ति, पूर्णता, प्रेम आदि के विचारों को 'सोऽहम्' के साथ जोड़ें। मन्त्र का उच्चारण करते समय शरीर को नकारें और परमात्मा के साथ अभिन्नता को स्वीकार करें।
(१३)
"किसी ऐसे आसन पर बैठ जायें, जो न बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा। हाथों को अपनी गोद में रख लें। अपने मन को स्थिर रखने के लिए नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को केन्द्रित करें । प्राण के प्रवाह-पथ (नाड़ियों) को शुद्ध करने हेतु पहले क्रम से पूरक, कुम्भक और रेचक करें। फिर क्रम बदल दें। अर्थात् पहले अँगूठे से दायें नासारन्ध्र को बन्द करके बायें नासारन्ध्र से पूरक करें। फिर अनामिका और कनिष्ठिका के बायें नासारन्ध्र को बन्द करके कुम्भक करें। फिर अँगूठे को हटा कर दायें नासारन्ध्र से श्वास निकाल दें। अब क्रम बदलते हुए दायें नासारन्ध्र से श्वास लें, कुम्भक करें और बायें नासारन्ध्र से श्वास निकाल दें। अपनी इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास करें।
"हृदय में कमल की डण्डी के पतले सूत्र के समान 'ॐ' का चिन्तन करें। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जायें और उसमें घण्टानाद के समान स्वर स्थिर करें। इस स्वर का ताँत टूटने न पाये। इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय १०-१० बार 'ॐ' के उच्चारण-सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से एक महीने के अन्दर ही प्राणवायु वश में हो जायेगी। इसके बाद ऐसा चिन्तन करें कि हृदय एक कमल है। वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थिर है कि उसकी डण्डी ऊपर की ओर और मुँह नीचे की ओर है। अब ध्यान करें कि उसका मुख ऊपर की ओर खिल गया है, उसके आठ दल हैं और उसके बीचोंबीच नीले रंग की एक अत्यन्त सुकुमार कर्णिका है। इस कर्णिका में क्रम से सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि का न्यास करें तथा अग्नि के अन्दर मेरे (श्री कृष्ण के) एक-एक अंग का ध्यान करें। अपने मन को मेरे एक-एक अंग में लगायें। मन के द्वारा इन्द्रियों को उनके विषयों से खींच लें और मन को बुद्धि की सहायता से मुझमें ही लगा दें। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे, तब मन को खींच कर एक स्थान में स्थिर करें और मेरे अन्य अंगों का चिन्तन करने के बजाय केवल मेरे मुस्कराते हुए मुख का ध्यान करें। जब ऐसा होने लगे, तो मन को वहाँ से हटा कर आकाश में स्थिर करें। इसके बाद आकाश का भी चिन्तन त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जायें और मेरे सिवा किसी भी अन्य वस्तु का चिन्तन न करें। जब मन इस प्रकार स्थिर हो जाता है, तब आप अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगेंगे।"
(श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में उद्धव द्वारा पूछे गये प्रश्न के भगवान् कृष्ण प्रदत्त उत्तर का एक अंश)
विषयानुक्रमणिका
१. ध्यान- आपका एकमात्र कर्तव्य 17
५. एकाग्रता के व्यावहारिक अभ्यास 27
१६. योगसार उपनिषद् के अनुसार ध्यानयोग 45
१७. वेदान्तसार उपनिषद् के अनुसार ध्यान में बाधाएँ 50
१८. ध्यानयोग का सार-संक्षेप 51
४. धारणा (एकाग्रता) की शक्ति 63
२६. मन समाधि में विगलित हो जाता है 76
२९. सब-कुछ है अखण्ड एकरस स्वरूप 78
३३. जहाँ वाणी की पहुँच नहीं है 80
३५. मैं नीरवता में निवास करता हूँ 81
३७. मेरा शरीर आनन्द से लबालब भरा हुआ है 82
३८. रोग ! तुम्हारा स्वागत है 82
४०. लघु 'मैं' परम दीप्ति से एकाकार हो गया 83
११. सभी आत्माओं में अन्तर्निहित एकत्व का साक्षात्कार करें 93
१६. वेदान्ती ध्यान के लिए सूत्र 94
१८. निर्गुण ध्यान के लिए सूत्र 95
२०. मैं कितना स्वतन्त्र हूँ 96
२३. मैं विज्ञानघन ब्रह्म हूँ 98
२४. मैं स्वतन्त्र ब्रह्म हूँ 98
२६. मैं निरावरण ब्रह्मस्वरूप हूँ 99
३०. मैं चिन्मात्र-स्वरूप हूँ 100
३२. मैं आनन्दघन स्वरूप हूँ 101
३३. -रहित ब्रह्म हूँ मैं माया- 101
३४. मैं निराकार, निर्गुण ब्रह्म हूँ 102
३५. मैं त्रिगुणातीत ब्रह्म हूँ 102
२. ब्राह्ममुहूर्त में ध्यान के लाभ 119
३. सांसारिक विचार तथा ध्यान 119
४. समाधि-अवस्था में प्रवेश 119
५. भगवान् हरि तथा एकाग्रता का पदार्थ 120
९. मन्त्र - साधना के अनुभव 126
११. सहज समाधि तथा निर्विकल्प-समाधि 127
१४. मनन तथा अतिचेतनावस्था का अनुभव 128
१६. प्रज्ञा का दिव्य नेत्र - प्रातिभज्ञान 129
समाधि तथा आध्यात्मिक अनुभव 130
ध्यानयोग
प्रथम अध्याय
ध्यानयोग की व्याख्या
१. ध्यान- आपका एकमात्र कर्तव्य
ध्यान आपका एकमात्र कर्तव्य है। आप अपने जीवन के लक्ष्य-ईश्वर- साक्षात्कार — को प्राप्त करें; तभी जीवन सार्थक हो सकेगा। ईश्वर-साक्षात्कार-रूपी मार्ग के कई पड़ाव हैं— शुद्धता, एकाग्रता, चिन्तन, मनन, ध्यान, आध्यात्मिक बोध, तादात्म्य (अभिन्नता), तल्लीनता तथा मोक्ष। सेवा करके अपने को शुद्ध बनायें और फिर एकाग्रता तथा ध्यान के पड़ावों से होते हुए अपने लक्ष्य मोक्ष तक पहुँचें।
ध्यान के लिए समय
ब्राह्ममुहूर्त में ब्रह्म-विचार करें। ब्राह्ममुहूर्त में अपने से प्रश्न करें— 'मैं कौन हूँ?' ब्राह्ममुहूर्त में किया गया एक घण्टे का ध्यान दिन के किसी अन्य समय में छह घण्टों तक किये गये ध्यान के बराबर है।
यदि आप प्रातः चार बजे उठ जायें, तो आपको भोर के समय प्रार्थना-ध्यान के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा। आप अपने व्यक्तित्व को सत्त्व से आवेशित कर लेंगे। दैनन्दिन जीवन की समस्याओं से जूझने के लिए आपको पर्याप्त शक्ति मिल जायेगी। ध्यान के लिए प्रातःकाल सर्वाधिक उपयुक्त है। इस समय मन राग-द्वेष से प्रभावित नहीं रहता (जैसे कि अन्य समयों में रहता है)। तब आप ध्यान करके तथा स्तोत्र, भजन- श्लोकों (यथा ‘अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे') का पाठ करके मन को सत्त्व से परिपूरित कर सकते हैं। हमेशा इसी तरह के पवित्र विचारों का चिन्तन करते रहें।
प्रारम्भिक अभ्यासियों को ध्यान का अभ्यास लम्बे समय तक नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे अपना अभ्यास-काल बढ़ाइए, ताकि आप दीर्घ काल तक ध्यान की स्थिति में रहने का लक्ष्य प्राप्त कर सके। अवकाश-प्राप्त व्यक्तियों को ध्यान के लिए अधिक समय देना चाहिए। परन्तु यदि प्रारम्भिक अभ्यासियों को लम्बे समय तक ध्यान का अभ्यास करने को कहा जाये, तो वे घबरा जायेंगे; इसीलिए मैं कहता हूँ- "थोड़ा ध्यान करें।" ऐसा कहने के पीछे मेरा उद्देश्य उन्हें ध्यान के लिए प्रोत्साहित तथा प्रेरित करना है।
ध्यान की विधि
मन प्रतिक्षण धोखा देता रहता है। अतः कम-से-कम अब तो जग जायें और सत्संग, स्वाध्याय तथा ध्यान करते हुए आत्मा के स्वरूप के बारे में निरन्तर अपने से प्रश्न करते रहें और इस प्रकार अपने विवेक को विकसित करें।
'ॐ' का ध्यान करें— “तजपस्तदर्थभावनम् ।" 'ॐ' सच्चिदानन्द है। 'ॐ' असीम है। 'ॐ' स्वतन्त्रता है, पूर्णता है। निर्गुण ब्रह्म के इन दैवी लक्षणों का ध्यान करें।
आत्मा के सत्, चित् और आनन्द (सच्चिदानन्द) स्वरूप का ध्यान करें। यदि आप यह ध्यान न कर सकें तो सूर्य, प्रकाश, सर्वव्यापी आकाश या वायु का ध्यान करें। हृदय में चमकते हुए प्रकाश का, समय-समय पर स्वप्न में दिखायी पड़ने वाले चित्रों का ध्यान करें । सन्त-महात्माओं या अपने गुरु के रूप का ध्यान करें। जो आपके मन को रुचिकर लगे, उसका ध्यान करें। अपने पिता और उनके गुणों का भी ध्यान कर सकते हैं।
कुछ मिनटों तक सामान्य ध्यान का अभ्यास करें। इस अभ्यास से आपको पता चल जायेगा कि वास्तविक शान्ति और परमानन्द आपके अन्दर ही हैं। चित्तवृत्तियों को समेट लें- “प्रत्यगात्मानं ईषत् आवृत्त चक्षुः ।" अपने इष्ट-मन्त्र का बार-बार उच्चारण करें। मन इन्द्रियों के विषयों की ओर न जाये तथा वृत्ति रहित हो। आप परम शान्ति और आनन्द का अनुभव करेंगे। इस ध्यान का नियमित रूप से अभ्यास करें।
"नामरूपं न ते न मे । "
'अहं आत्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः ।'
इन श्लोकों के निहितार्थ का बार-बार मनन करें। इनमें निहित विचार आपको शक्ति प्रदान करेंगे। आप थोड़ा भी मनन करेंगे, तो भी आपको कुछ-न-कुछ शक्ति प्राप्त होगी।
आप पंचतत्त्वों से निर्मित शरीर नहीं हैं। इस बात का स्मरण बार-बार करें। इस पर मनन करें। मनन-ध्यान के द्वारा आपको आत्मा का साक्षात्कार करना है। "आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान है। आत्मा को प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है।" यह आपका वास्तविक स्वरूप है। इस संसार में आत्मा की तरह कोई पदार्थ नहीं है।
ध्यान करें और गायें - "शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सोऽहम् । सच्चिदानन्दस्वरूपोऽहम्।”
शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए आसन-प्राणायामों का अभ्यास करें। इनसे रोग भी दूर होंगे तथा एकाग्रता ध्यान के अभ्यास करने में सहायता मिलेगी।
ब्राह्ममुहूर्त में उठ कर ध्यान करें। दिव्य तत्त्व का चिन्तन-मनन करने के लिए यह समय सर्वोत्तम है। इस समय मन शान्त रहता है। यह एक कोरे कागज की तरह होता है। इसको किसी भी तरह रूपान्तरित किया जा सकता है। इस समय सांसारिक राग-द्वेष इसको प्रभावित नहीं कर पाते।
ब्राह्ममुहूर्त में ॐ (दीर्घ प्रणव) का १०-१२ बार उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार उच्चारण करने से सभी कोशों में सुसंगत प्रदोलन होने लगते हैं।
गहन ध्यान करें। सतत ध्यान करें। प्रारम्भ में लगातार ध्यान करना कठिन जान पड़ेगा; परन्तु अभ्यास करना न छोड़ें। आप असीम आनन्द का अनुभव करेंगे। ध्यान का समय बढ़ाते जायें। धीरे-धीरे आप गहन और सतत ध्यान की स्थिति में पहुँच जायेंगे।
सत्, चित् और आनन्द के अमूर्त गुणों का ध्यान करें। सदैव मन में इनका विचार बनाये रखें। यह विचारों की अमूर्त पृष्ठभूमि है। आप ईश्वर के आकार पर भी ध्यान कर सकते हैं। यही सगुण उपासना है। भगवान् के चित्र का मानस-दर्शन करें। उनके मुख-कमल, चक्र, चरणारविन्दों का एक-एक करके ध्यान करें। मन नहीं भागेगा।
मन को बहिर्गामी नहीं होना चाहिए। अपने अन्तरतम में निवास करने वाले ईश्वर पर मन को स्थिर करने से आप अन्तर्मुखी हो जायेंगे।
आप मन की ज्योतियों का ध्यान कर सकते हैं। स्वप्नों में या सूक्ष्म दृष्टि से दिखायी पड़ने वाले दिव्य पदार्थों का भी ध्यान कर सकते हैं। आप राग-द्वेष से मुक्त किसी सन्त-महात्मा के रूप का भी ध्यान कर सकते हैं। "यथाभिमत ध्यानाद्वा" आप अपनी रुचि की किसी भी वस्तु का ध्यान कर सकते हैं।
एक शिष्य ध्यान से सम्बन्धित मार्ग-निर्देशन प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास ने उससे भगवान् राम का ध्यान करने के लिए कहा। शिष्य ने उत्तर गया। दिया- "मुझे भगवान् राम का ध्यान करना बहुत कठिन मालूम पड़ता है।"
"क्यों ?" ने —गुरु ने पूछा।
"क्योंकि मुझे अपनी भैंस से अत्यधिक प्रेम है।"
गुरु ने उत्तर दिया—“तब तुम उसी भैंस का ध्यान करो।”
शिष्य भैंस का ध्यान करने लगा। तीन दिन बीत गये। गुरु ने कहा- “अब तो
(ध्यान कक्ष से) बाहर आओ।"
"मैं कैसे बाहर आऊँ?"-शिष्य ने कहा।
“क्यों, क्या हुआ?”
"मैं स्वयं ही भैंस बन गया हूँ। मैं दरवाजे से निकल ही नहीं सकता।'
वस्तुतः शिष्य मन की गहन एकाग्रता के कारण भैंस से एकाकार हो गया था। तब गुरु ने उससे भगवान् विष्णु के रूप का ध्यान करने को कहा। फिर शिष्य ध्यान करते-करते गहन समाधि की स्थिति में पहुँच गया।
साधना-पथ पर बहुत से अवरोध हैं। इनको पराभूत करना होगा। निद्रा सदैव बाधा उत्पन्न करती है। रात्रि के समय हलका भोजन लें। जब नींद आने लगे, तो चेहरे पर ठण्ढे पानी के छींटे मारें। भस्त्रिका करें। उठ कर खड़े हो जायें और कुछ देर तक खड़े-खड़े ही जप करें। ॐ का १०-१२ बार उच्चारण करें। ध्यान कक्ष में तेज रोशनी होने दें। इन सभी या कुछ विधियों का एक-साथ प्रयोग करके देखें। निस्सन्देह इस प्रकार नींद काबू में आ जायेगी। एक दूसरा भी उपाय है। डोरी से अपनी चोटी को दीवाल में लगी किसी कील से बाँध लें। अब ध्यान करें। नींद आयेगी, तो वह कील आपको अपनी तरफ खींच कर जगा देगी।
जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठते हैं, तरह-तरह के विचार मन में आने लगते हैं। परेशान न हों। आपने अब तक उन्हें खूब छूट दी है। अब वे आपसे लड़ने के लिए आये हैं; क्योंकि अब आप उन सबको नष्ट कर देना चाहते हैं। यह स्वयं आध्यात्मिक विकास का लक्षण है। यदि आप स्थिरता से नियमित साधना कर रहे हैं, तो ये नकारात्मक संस्कार स्वतः समाप्त हो जायेंगे। तब आप ध्यान और समाधि की स्थितियों में प्रवेश करेंगे।
अविद्या, काम और कर्म ग्रन्थियाँ हैं। आद्य अज्ञान अविद्या है। इस अज्ञान से काम (कामना) उत्पन्न होता है। शुद्ध परम तत्त्व में किसी प्रकार की कामना नहीं होती। कामना से कर्म उत्पन्न होते हैं। कामना ही अपूर्णता है। आप बाह्य पदार्थों में आनन्द खोजते हैं। जब अपूर्णता नहीं होती, कामनाएँ नहीं होतीं, तब आत्मानन्द का अनुभव होता है। यदि नियमित ध्यान की सहायता से आप इन कामनाओं को नष्ट कर सकें, तब पलक मारते ही आप इन ग्रन्थियों को काट सकते हैं।
आपको एक निश्चित समय पर नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए नियत समय पर ध्यान के लिए उपयुक्त मनःस्थिति अपने-आप बन जाती है। इसके अतिरिक्त धीरे-धीरे समय की अवधि बढ़ाते हुए आपको पूरे दिन ध्यान-भाव बनाये रखना चाहिए। तब आप शान्त, प्रसन्न और सन्तुलित हो जायेंगे। तब आप अधिक निपुणता से अधिक कार्य कर सकेंगे।
ध्यान की महिमा
आपको अभी से ध्यान का अभ्यास प्रारम्भ कर देना चाहिए। जब आप गर्भ में थे, तब आपने वचन दिया था कि आप ध्यान करेंगे और आत्मा का साक्षात्कार करेंगे। आप अपने वचनों को भूल हैं। यदि आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो थोड़ी निद्रा ही पर्याप्त होगी। थोड़ी ही देर के लिए किये गये ध्यान से ही बाद में अच्छी नींद आती है। स्वयं ध्यान से ही आपको स्फूर्ति प्राप्त होगी। अपने दैनिक कार्य करते हुए भी अपने को ध्यान की भावभूमि में अवस्थित रखें।
यदि मन किसी पदार्थ की ओर भागे, ऐन्द्रिक सुख की कामना करे, तो उससे कह दें — “जरा रुको! मैं तुम्हें ध्यान का परमानन्द प्रदान करूँगा। हे कामना! तुम अभी मेरा पीछा छोड़ो।" इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा करके आप अपने मन के प्रभाव को क्षीण कर सकते हैं। यदि प्रातः कालीन ध्यान से एक बार भी आपको परमानन्द का और परम शान्ति का अनुभव हो जाये, तो भगवान् के चरण-कमलों से मन को हटा पाना आपके लिए असम्भव हो जायेगा, तब एक दिन भी ध्यान न करना आपको खल जायेगा। अभी ध्यान करें। थोड़ा ही ध्यान करें। स्वयं देखें कि ध्यान से अनिर्वचनीय शान्ति प्राप्त होती है कि नहीं। आँखें बन्द करें तथा कृष्ण, राम, ईसामसीह, ॐ, अपने पिता या किसी का भी ध्यान करें।
'ॐ' का उच्चारण करें। अपनी आन्तरिक आत्मा के परमानन्द का आस्वादन करें। ध्यान नियमित रूप से करें। भोर के समय पहला ध्यान करें। स्नान करने के बाद दूसरी बार ध्यान के लिए बैठें। फिर सायंकाल ध्यान करें। सोने से पूर्व एक बार फिर ध्यान करें।
यदि आप एक अलग ध्यान-कक्ष का प्रबन्ध नहीं कर सकते, तो अपने कमरे का एक कोना ही ध्यान का अभ्यास करने के लिए सुरक्षित कर लें।
प्रतिदिन अपने दैनिक कार्य-कलाप करते हुए ध्यान का अभ्यास करें। यह आपका परम कर्तव्य है। इसकी उपेक्षा किसी भी परिस्थिति में न करें। प्रातः चार बजे उठ जायें। थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा कीर्तन करें, गीता या अन्य धर्मग्रन्थों का स्वाध्याय करें, फिर आत्म-विश्लेषण करें।
अपने सभी कार्यों को आध्यात्मिक पुट दें। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। प्रातः आधे घण्टे ध्यान करके दिन-भर गलत-सलत काम करने से बात नहीं बनेगी। इस स्थिति में ध्यान करके जो संस्कार बनेंगे, वे दिन के समय प्रायः नष्ट हो जायेंगे। आपको दिन-भर अध्यात्म की भावभूमि पर अवस्थित रहना है।
यदि आप ध्यान का नियमित अभ्यास कर रहे हैं, तो कठिनाइयाँ और भ्रम स्वतः ही नष्ट हो जायेंगे।
२. विविधता से परावर्तन
आत्म-निग्रह और आत्माभिव्यक्ति दो अलग-अलग विचार हैं। आत्माभिव्यक्ति प्रवृत्ति-मार्ग से या इस बहुरंगी संसार में व्यतीत किये जाने वाले जीवन से सम्बन्धित है। आत्म-निग्रह साधक को निवृत्ति-मार्ग से उच्चतम संघटन की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में, वह उसे सत्य की ओर वापस ले जाता । विविधता उत्पन्न करने वाली सृजनात्मक शक्ति की बहिर्मुखता समाप्त होती है, उसका उदात्तीकरण हो जाता है और वह एक आध्यात्मिक दीप्ति से प्रकाशित होने लगती है। आत्म-निग्रह द्वारा ही विविधता से हट कर एकता में केन्द्रित होना सम्भव है। आत्म-निग्रह सृजनात्मक विषयपरक बल के चेतन शक्ति में रूपान्तरित होने का द्योतक है। यही शक्ति वैयक्तिक ससीमता को पदार्थ-रहित चेतना के विस्तार में पुष्पित करती है। प्रकटीकरण का अर्थ है विविधता । प्रत्येक वैयक्तिक बल असीम सृजनात्मक बल की प्रतिकृति है और यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से विविधता के सर्जन की ओर उन्मुख रहती है। यही कारण है कि उन लोगों के लिए सर्जन की क्रिया को नियन्त्रित कर पाना कठिन होता है जो भौतिक शरीर में बहुत अधिक आसक्त रहते हैं। आत्म-साक्षात्कार की प्रक्रिया से सम्बद्ध हुए बिना वैश्व-स्वभाव को भली प्रकार निर्देशित करना कठिन हो जाता है। आध्यात्मिक साधक इस विषयनिष्ठ ऊर्जा के स्रोत में पहुँचता है तथा उसे परासत्ता की प्रशान्त भूमि में विसरित होने के लिए विवश करता है। जो व्यक्ति इस सृजनात्मक शक्ति के प्रवाह पर नियन्त्रण नहीं रखता, वह विविध सृष्टि की प्रक्रिया में उलझ जाता है। वह अपनी शाश्वत आत्मा के अद्वैत सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। यह इस विश्वजनीन नीति की मूल पृष्ठभूमि है कि परम सत्य की खोज में रत साधकों के लिए आत्म-निग्रह अत्यावश्यक है।
जिन्होंने मानव-जीवन के आध्यात्मिक स्वरूप को विवेकपूर्वक समझ लिया है, वे आत्म- बाहुल्य (self-multiplication) की साहजिक क्रिया से अपने को अलग रखते तथा सामान्य मानव-स्वभाव के क्रियाशील, भावनात्मक और बौद्धिक पक्षों के त्रिपक्षीय रूपान्तरण के माध्यम से अपनी अन्तर्निहित ऊर्जा को 'आध्यात्मिक आदर्श' के जागरूकतापूर्वक चिन्तन-मनन की ओर उन्मुख किये रहते हैं। ऐसे संघटित व्यक्तित्व वाले साधकों के पास विवेक, विश्लेषण तथा ध्यान की सशक्त क्षमताएँ होती हैं। छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार, जब शुद्धता तथा सत्त्व के गुणों में वृद्धि हो जाती है, तब स्मरण-शक्ति भी प्रखर होती है तथा आत्म-ग्रन्थि भी उच्छेदित होने लगती है। जिस संयमी साधक • अनन्त जीवन की परिपूर्णता में अपनी निर्माणात्मक शक्ति का विस्तार करना सीख लिया है, वही आत्म-साक्षात्कार की जटिल विधि को जानता और समझता है। ऐसा ही साधक आध्यात्मिक शक्ति की दीप्ति से चमकता रहता है तथा प्रकृति की विविध दुर्जेय शक्तियों का सामना कर सकता है। वह निर्भीक होता है। वह दिव्यता को प्राप्त अपनी ऊर्जा को आत्मा में केन्द्रित करके, उसकी सहायता से अहं के क्षेत्र से परे हो जाता है। वह दृश्य-प्रपंच को लाँघते हुए परम सत्ता के अन्तरतम में प्रवेश पा लेता है। आत्म-निग्रही की यह है महिमा !
विषयगत वृत्तियों का नियन्त्रण करने से परम तत्त्व की खोज के लिए संसार का त्याग करना सरल हो जाता है। एक वास्तविक संयमी साधक की पहचान यह है कि उसमें विशिष्टताओं (particularities) के प्रति अरुचि से उत्पन्न सांसारिकता के त्याग की भावना रहती है। वह गृहस्थों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता। उसका मार्ग परम ऐक्य का मार्ग है। रचनात्मक सामाजिक कार्यों का पथ उसके लिए नहीं है। अकेला, एकाकी ही वह दिव्य आदर्शों का स्मरण करता हुआ सतत निःस्वार्थपरता से आत्म-संघटन के कर्तव्य का पालन करता है। निःस्वार्थ सेवा साधक के व्यक्तित्व का परिष्कार करती है, उसके अहं को समाप्त करती है और उसे ब्रह्म-चिन्तन तथा ध्यान के उच्चतर जीवन के लिए तैयार करती है। सम्बन्धियों से सम्बन्ध-विच्छेद करना आवश्यक है; क्योंकि निवृत्ति-मार्ग में अल्पकालिक सम्बन्धों के लिए कोई स्थान नहीं है।
प्रज्ञा प्राप्त करने की पात्रता
जो प्रज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, उसे 'उचित समय पर' यह अवश्य प्राप्त होगी। साधक द्वारा किये गये प्रयास तथा समय का व्यतिक्रम एक-दूसरे से भिन्न नहीं है। दोनों साथ-ही-साथ कार्य करते हैं। इसका कारण यह है कि ईश्वर तथा व्यक्तिगत प्रयास भी परस्पर अभिन्न तथा अन्योन्याश्रित हैं। ये एक ही क्रिया-शक्ति के दो नाम हैं।
श्री शंकराचार्य के अनुसार, परम सत्ता के रहस्यों में दीक्षित होने के लिए साधक को विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा मुमुक्षुत्व की अनुशासनिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जब तक साधक में इन गुणों का भली-भाँति विकास न हो जाये, तब तक उसे परम तत्त्व की सत्यता की दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। आजकल साधकों में विवेक और वैराग्य की झलक मात्र ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसे साधक बहुत कम हैं जो परम मोक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी का चिन्तन नहीं करते; जो इस संसार और सांसारिक पदार्थों को तृण से अधिक महत्त्व नहीं देते तथा जो सदैव अपने मूर्त अस्तित्व के बन्धन से मुक्त हो कर मोक्ष प्राप्त करने के विषय में ही चिन्तन करते रहते हैं। मोक्ष का वास्तविक अर्थ समझ पाना सरल नहीं है। संसार के अपरिष्कृत मनुष्यों के लिए यह कैसे सम्भव है कि पार्थिव सत्ता तथा सांसारिक कार्यकलापों की निस्सारता को समझ सकें? कभी-कभी तो साधकों में भी यह इच्छा बलवती हो उठती है। कि वे इस संसार में कुछ ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्य कर दिखायें, जिसे पहले किसी ने न किया हो। ऐसे व्यक्तियों में कभी भी मोक्ष की वास्तविक कामना नहीं हो सकती। वे ब्रह्मविद्या प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। जो किसी बात की चिन्ता नहीं करते, जिन्हें सांसारिक रीतियाँ आकर्षित नहीं कर पात, जो अपने में उचित ज्ञान का उदय हो जाने के कारण शान्त और चुप रहते हैं, जो संसार के विविध स्वभावों वाले प्राणियों के बीच भी सदा एक समान रहते हैं, जिनमें विभ्रान्त कर देने वाले सांसारिक कार्यकलाप विक्षोभ नहीं उत्पन्न कर पाते, जिन्हें जीवन की हलचल विचलित नहीं करती, जो जीवन-मृत्यु दोनों से ही अप्रभावित रहते हैं तथा जिन्हें सांसारिक घटनाओं से लेना-देना नहीं रहता- केवल ऐसे ही उत्तम अधिकारियों में परम तत्त्व का परम ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता होती है। यदि साधकों के मन में ब्रह्म-साक्षात्कार से इतर कोई दूसरी इच्छा रंचमात्र भी है, तो वह गुरु द्वारा प्राप्त वैदिक शिक्षा के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकेगा। उसके मन में तरह-तरह के भ्रम उत्पन्न होते रहेंगे और वह सदैव अन्यमनस्कता की स्थिति में रहेगा। उसका मन वैदिक ध्यान से हट जायेगा। ब्रह्म-साक्षात्कार के अतिरिक्त कोई अन्य कामना साधक के मन में नहीं होनी चाहिए। 'कैसे साक्षात्कार हो सके इसके अतिरिक्त उसे कुछ चिन्तन नहीं करना है। उसके प्रत्येक विचार, वाणी, कर्म—यही नहीं, प्रत्येक श्वास में उसके इसी चिन्तन की झलक मिलनी चाहिए। ऐसा ही साधक वेदान्त के ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है।
ध्यान के लिए मार्ग-निर्देशन
उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति से सम्बन्धित विचारों की शक्ति को संकेन्द्रित करना ध्यान है। ध्यान की प्रक्रिया का प्रारम्भ द्वैत की सत्ता में विश्वास रखने के साथ होता है। इस विश्वास के अभाव में ध्यान चिन्तन मात्र बन कर रह जायेगा और एकाग्रता नहीं रह पायेगी; ध्यान का प्रारम्भ द्वैत-भाव से तथा अन्त सत्ता की एकता की गौरवमयी चेतना से होता है।
अस्तित्व की सत्यता तथा वास्तविकता में आस्था होना इस कारण आवश्यक है कि समूचा ब्रह्माण्ड क्रमिक रूप से उच्चतम ब्रह्म का ही मूर्त रूप धारण करता है। ध्याता से पूर्णतः असम्बद्ध श्रेष्ठतम लोकातीत सत्ता का साक्षात्कार होना असम्भव है। सत्य एक सर्वव्यापी उपकरण है। ध्येय तथा ध्याता में अत्यन्त निकटतम सम्बन्ध होता है। ध्येय ध्याता का सारतत्त्व ही होता है, इस प्रकार 'असीम तत्त्व' के साक्षात्कार की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। लोकोत्तर आध्यात्मिक पूर्णता के परमानन्दमय क्षेत्र तक ले जाने वाली सीढ़ी का एक डण्डा संसार ही है।
इस प्रकार साधक को यह बोध हो जाता है कि प्रकृति की वर्तमान शक्तियाँ उसके विरोध में नहीं हैं। उनसे मित्रता करके और उनका उपयोग करते हुए ध्यान में सहायता प्राप्त की जा सकती है। कौन कह सकता है कि कठोर भूमि, तरल जल, तप्त अग्नि, बहती हुई वायु और शून्य आकाश में अन्तर नहीं है? जब तक व्यक्ति को अपनी सम्बन्धात्मक विशिष्टता का भान रहेगा, तब तक यह अन्तर रहेगा ही। मौसम में पाया जाने वाला अन्तर, मानव बुद्धि की विभिन्न कोटियाँ, मूर्त चेतना के कोशों की विभिन्न आवश्यकताएँ, तरह-तरह की भावनाएँ, सुख-दुःख, मनोवेग और इच्छाएँ — ये सब सत्य के प्रकटीकरण की प्रक्रिया में पायी जाने वाली विभिन्नताओं की ही सूचना देते हैं। ब्रह्म प्रत्येक वस्तु में समान रूप से व्यक्त नहीं होता। दिव्य आत्माओं, अवतारों तथा सन्त-महात्माओं से यह बहुत स्पष्टता से व्यक्त होता है। साधारण मनुष्यों में यह इतनी स्पष्टता से व्यक्त नहीं होता। अचेतन पदार्थों में इसकी अभिव्यक्ति बहुत कम होती है। प्रकृति की कार्य-प्रणाली के नियमों तथा योजनाओं का पूरा ज्ञान होने से गहन ध्यान द्वारा ब्रह्म-चेतना के साक्षात्कार की प्रक्रिया में गति आ जाती है।
पर्वत-शिखरों पर, जल के विशाल विस्तार वाले क्षेत्रों तथा मेघाच्छन्न मौसम में वायुमण्डलीय विद्युत् उत्पन्न होती रहती है। अतः ये समय तथा स्थान ध्यान के लिए अत्यन्त उपयुक्त होते हैं। ये प्रभावशाली ध्यान से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं। खुले आकाश का विस्तार भी ध्यान करने में सहायक सिद्ध होता है। सँकरे स्थान विस्तारित अस्तित्व की चेतना को बाधा पहुँचाते हैं। अस्तित्व के विस्तार के लिए ऐसे स्थान सहायक नहीं हैं।
उत्तराखण्ड में सन्त-महात्माओं तथा देवताओं ने निवास तथा ध्यान किया है; अतः ध्यान के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। हिमालय तथा पवित्र गंगा से निकलने वाली उदात्त आध्यात्मिक तरंगें ध्यान के लिए अत्यन्त सहायक हैं। हिमालय के शिखरों तक विस्तारित हरिद्वार • ऊपर का समस्त क्षेत्र ध्यान के लिए एक श्लाघ्य क्षेत्र है। सन्त-महात्माओं ने इस क्षेत्र में तपस्या-ध्यान किया है और अमिट आध्यात्मिक प्रभाव-तरंगें छोड़ गये हैं।
ध्यान करने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठना सर्वोत्तम है। उत्तर दिशा में एक प्रभावकारी चुम्बकीय शक्ति होती है। समस्त परमानन्द भी इसी दिशा में उपलब्ध होता है।
रात्रि १२ बजे और प्रातः ४ बजे के बीच का समय ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। इस समय पूर्ण शान्ति तथा शीतलता रहती है। वातावरण में संघटनकारी स्पन्दन उपस्थित रहते हैं। अन्धकार में समस्त दृश्य-प्रपंच समष्टि के रूप में दिखायी पड़ने लगता है। (दूसरी ओर, प्रकाश हमें संसार की विविधता देखने के लिए विवश करता है) सूर्य का प्रकाश यां अन्य अप्राकृतिक प्रखर प्रकाश (जैसे गैस का प्रकाश) ध्यान करने के लिए उपयुक्त नहीं है; क्योंकि उनसे मन में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ध्यान के लिए अँधेरे स्थान उपयुक्त हैं। चाँदनी रात भी इस हेतु उपयुक्त है।
ध्यान करते समय शरीर में शक्तिशाली विद्युत्-तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस समय हाथ-पैरों को फैला कर रखने से तरंगें उँगलियों के अग्रभाग से निकल कर हवा में विलीन हो जाती है। अतः ध्यान करते समय दोनों हाथों की उँगलियाँ परस्पर एक-दूसरे से मिली रहनी चाहिए या घुटनों को स्पर्श करती रहनी चाहिए। इस समय पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या स्वस्तिकासन में बैठने से इस तरंगों का शरीर में ही परिसंचरण होता रहता है।
पृथ्वी में विद्युत् ऊर्जा को शरीर से खींच लेने की क्षमता होती है; अतः ध्यान करते समय व्याघ्र चर्म या मृगछाला पर बैठना चाहिए, ताकि शरीर की ऊर्जा नष्ट न हो तथा वह अधिक मात्रा में उत्पन्न हो सके।
मेरुदण्ड झुके होने की स्थिति में किसी प्रकार की एकाग्रता सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि इस स्थिति में प्राण-तरंगों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। अतः ध्यान करते समय मेरुदण्ड सीधा रहना चाहिए।
साधक में या तो प्रबुद्ध ज्ञान होना चाहिए या दृढ आस्था होनी चाहिए। इन दोनों के अभाव में परम सत्ता का ध्यान नहीं किया जा सकता। किसी उन्नत आध्यात्मिक महापुरुष की संगति करके उनसे सहायता प्राप्त किये बिना ध्यान सम्भव नहीं है। अपवाद स्वरूप ही इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता नकारी जा सकती है। किसी अनुभवी सन्त महात्मा की संगति के अभाव में असीम तत्त्व के साथ जीवात्मा को संस्वरित करने की प्रविधि का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता । स्वाध्याय करने से साधना में गति तो आती है, परन्तु 'अशुभ' का सामना करने की शक्ति महापुरुषों की संगति से ही प्राप्त होती है।
ध्यान के सबसे भयानक शत्रु हैं— कामुकता तथा क्रोध। ये क्षण मात्र में ही दीर्घ काल तक किये गये ध्यान से प्राप्त शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। अतः साधक को इन दो नकारात्मक शक्तियों से सावधान रहना चाहिए।
नेत्रों तथा कानों को बन्द कर लेने के पश्चात् अनुभव के क्षेत्र से पूरा जगत् पलायन कर जाता है। ध्वनियों तथा रंगों से यह सारा जगत् निर्मित है। जब ये दोनों नहीं होते, तो कुछ भी शेष नहीं रहता ।
ध्यान के अभ्यासी साधक को बाह्य जगत् में होने वाली घटनाओं में रुचि नहीं लेनी चाहिए। संसार सुखी है या दुःखी — इसकी चिन्ता साधक को क्यों हो? साधक की दृष्टि में उसके अपने व्यक्तित्व का कोई महत्त्व नहीं होता। वह असीम पूर्णता के ही ध्यान में सतत निमग्न रहता है।
परम असीम तत्त्व के अतिरिक्त अन्य किसी को प्राप्त करने की इच्छा न रखें। यह सबसे महत्त्वपूर्ण बात है। मोक्षप्रिय ने कहा- “हे परम प्रिय गुरुदेव ! आप कृपा करके संक्षेप में एकाग्रता के बारे में पूरी जानकारी दें।"
३. एकाग्रता (धारणा)
मोक्षप्रिय ने कहा-''हे परम प्रिय गुरुदेव ! आप कृपा करके संक्षेप में एकाग्रता के बारे में पूरी जानकारी दें ।''
गुरुदेव ने उत्तर दिया – “धारणा ही एकाग्रता है। ईश्वर, ब्रह्म या किसी स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ पर मन को लगातार टिकाये रखना धारणा है।
"मन सदैव भागता रहता है। यह ऐन्द्रिक पदार्थों के प्रति आकर्षित हो कर सदैव उन्हीं का चिन्तन करता है और उन्हीं की ओर दौड़ता है। पलक मारते ही यह बन्दरों की तरह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर छलाँग लगा देता है। यह इसका स्वभाव है।
“वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को किसी पदार्थ या विचार-बिन्दु पर टिकाना धारणा है। धारणा ही एकाग्रता है।
"धारणा का अभ्यास एक दिन, सप्ताह या मास में पूरा नहीं हो जाता। गहन आस्था तथा असीम उत्साह के साथ दीर्घ काल तक धारणा का अभ्यास करना चाहिए।
"ब्रह्मचर्य, वैराग्य और निष्कामता ——ये वैराग्य की तीन पूर्वापेक्षाएँ हैं। ऊर्जा को ऐन्द्रिय-छिद्रों से नहीं बहने देना चाहिए।
"एकाग्रता के लिए यम-नियम का पालन भी आवश्यक है। आसन पर स्थिर बैठे। प्राणायाम की सहायता से अपने श्वास-प्रवाह को नियमित तथा नियन्त्रित करें। ऐन्द्रिय-पदार्थों में अपनी इन्द्रियों को लिप्त न रहने दें (प्रत्याहार का अभ्यास करें)। इसके बाद आप एकाग्रता का अभ्यास कर सकेंगे।
"हे मोक्षप्रिय ! एकाग्रता या धारणा में सुस्थित होने के बाद ध्यान और समाधि की अवस्थाओं में प्रवेश करना अत्यन्त सहज तथा सरल हो जायेगा।
"एकाग्रता दो प्रकार की होती है—स्थूल और सूक्ष्म । प्रारम्भिक अभ्यासी के लिए किसी रूप पर स्थूल एकाग्रता करना उपयुक्त होगा। बाद में वह किसी सूक्ष्म विचार (जैसे सुन्दरता, शुद्धता, शान्ति, परमानन्द) पर एकाग्रता का अभ्यास कर सकता है।
"दीवाल पर बने हुए किसी काले बिन्दु, मोमबत्ती की लौ, भगवान् के चित्र, नासिका में प्रवाहित होता हुआ 'सोऽहम्' श्वास, सूर्य, चन्द्रमा या तारों पर एकाग्रता का अभ्यास करें।
“एकाग्रता के अभ्यास में नियमित रहना बहुत आवश्यक है। अपने अभ्यास में एक दिन के लिए भी न चूकें। निश्चित समय पर निश्चित अवधि तक प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करें। अपने आहार का ध्यान रखें। सात्त्विक तथा हलका आहार लें। अपने संगी-साथियों के चुनाव में सतर्कता बरतें। दुर्जनों का संग न करें। गुरु और ईश्वर के प्रति आस्था तथा श्रद्धा रखें। हे साधना-धीर! सत्य-प्रेमी ! एकाग्रता के अभ्यास में आपको अवश्य सफलता मिलेगी।"
४. एकाग्रता का अभ्यास
शरीर के बाहर या अन्दर किसी पदार्थ पर मन को केन्द्रित करें। कुछ देर तक लगातार मन को केन्द्रित किये रहें। यही एकाग्रता है। यह अभ्यास प्रतिदिन करें।
पहले सदाचरण से मन को शुद्ध करें। इसके बाद एकाग्रता का अभ्यास करें। मन शुद्ध न हो, तो एकाग्रता का अभ्यास करना व्यर्थ है। कुछ तान्त्रिक (occultists) एकाग्रता का अभ्यास कर लेते हैं; परन्तु उनका चरित्र अच्छा नहीं होता, इसलिए वे अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति स्थिर हो कर आसन पर बैठ सकता है, जिसने प्राणायाम के अभ्यास द्वारा अपनी नाड़ियों तथा प्राणमय कोश को शुद्ध कर लिया है, वह एकाग्रता का अभ्यास सफलतापूर्वक कर सकता है। सभी विकर्षणों को हटा दें, एकाग्रता गहन हो जायेगी। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखा है, वह एकाग्रता का सफल अभ्यास सरलतापूर्वक कर सकता है।
कुछ मूर्ख, अधीर साधक आचारशास्त्र का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना ही एकाग्रता का अभ्यास करने लगते हैं। यह एक भारी भूल है। नैतिक पूर्णता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है।
एक वैज्ञानिक अपने मन को एकाग्र करके कई वस्तुओं का आविष्कार करता है। एकाग्रता की सहायता से वह अपने स्थूल मन की परतों को अनावृत करता है। वह उच्चतर मन के क्षेत्रों में प्रवेश करके उच्च ज्ञान प्राप्त करता है। वह अपने मन की समस्त ऊर्जाओं को संकेन्द्रित (एकाग्र) करके उनका उन पदार्थों के लिए उपयोग करता है, जिन पर वह शोध कर रहा होता है।
जो साधक अपनी इन्द्रियों को उनके पदार्थों से असम्बद्ध कर लेता है, वह एकाग्रता का सफल अभ्यास कर सकता है। आपको आध्यात्मिक मार्ग पर एक-एक सोपान को पार करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। सदाचरण, ध्यान के आसन में बैठने का अभ्यास, श्वास- नियन्त्रण, प्रत्याहार—ये ध्यान-रूपी भवन की नींव के पत्थर हैं। नींव के पत्थर मजबूत होंगे, तो भवन भी मजबूत तैयार होगा।
आपमें यह क्षमता होनी चाहिए कि एकाग्रता के विषय की अनुपस्थिति में भी आप उसका मानस-दर्शन कर सकें। जब भी आप चाहें, क्षण मात्र के अन्दर ही उसका मानसिक चित्र आपकी मन की आँखों के सामने आ जाना चाहिए। यदि आप सफलतापूर्वक एकाग्रता का अभ्यास कर लेते हैं, तो ऐसा करने में आपको बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अभ्यास के प्रारम्भिक चरण में आप घड़ी की टिक-टिक या मोमबत्ती की लौ या अच्छे लगने वाले किसी भी पदार्थ पर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कर सकते हैं। यह स्थूल एकाग्रता है। एकाग्रता तभी सम्भव हो सकती है, जब कोई ऐसी वस्तु उपलब्ध हो जिस पर मन को टिकाया जा सके। प्रारम्भ में किसी भी वस्तु (जो आपको अच्छी लगती हो) पर मन को केन्द्रित किया जा सकता है। शुरू-शुरू में मन को ऐसी वस्तु पर केन्द्रित करना बहुत कठिन हो जाता है, जिसमें मन की कोई रुचि न हो।
पद्मासन में बैठें। नासिकाग्र-बिन्दु पर अपनी दृष्टि को केन्द्रित करें। आँखों पर जोर न डालें। नासिकाग्र-बिन्दु को सहजतापूर्वक देखते रहने का अभ्यास करें। प्रारम्भ में इस अभ्यास को एक मिनट तक करें। धीरे-धीरे करके अभ्यास का समय लगभग आधा घण्टे तक बढ़ा दें। इस अभ्यास से मन स्थिर होता है तथा एकाग्रता की क्षमता विकसित होती है। यह अभ्यास चलते-चलते भी किया जा सकता है।
पद्मासन में बैठें। भ्रूमध्य-बिन्दु पर मन को केन्द्रित करें। मन पर जोर न डालें। यह अभ्यास आधा मिनट तक करें। अभ्यास की विधि को धीरे-धीरे करके लगभग आधा घण्टे तक बढ़ा दें। अभ्यास करते समय सहजता का ध्यान रखें। किंचित् भी तनाव उत्पन्न न करें। इस अभ्यास से मन की चंचल प्रकृति को नियन्त्रित किया जा सकता है। यह अभ्यास करते समय दृष्टि मस्तक के सामने ही हड्डी की ओर होती है। आप अपनी रुचि, स्वभाव और क्षमता के अनुसार अभ्यास के लिए नासिकाग्र-बिन्दु या भ्रूमध्य-बिन्दु में से किसी एक को चुन सकते हैं।
यदि आप अपनी एकाग्रता-शक्ति का विकास करना चाहते हैं, तो आपको सांसारिक कार्यकलापों में अपनी व्यस्तता को कम करना होगा। आपको प्रतिदिन कम-से-कम दो घण्टे तक मौनव्रत धारण करना होगा।
जब तक मन एकाग्रता के विषय पर भली प्रकार केन्द्रित न होने लगे, तब तक अभ्यास करते जायें। जब मन इस विषय से भागने लगे, तब जागरूकतापूर्वक इसे वापस ला कर इस विषय पर केन्द्रित करें।
जब एकाग्रता गहन हो जाती है, तब इन्द्रियों की कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। जो साधक प्रतिदिन तीन घण्टे तक एकाग्रता का अभ्यास करता है, उसमें अतीन्द्रिय-शक्ति बहुत अधिक मात्रा में होती है। उसकी इच्छा-शक्ति भी प्रबल होती है।
एक शिल्पी तीर बनाया करता था। एक दिन वह अपने कार्य में बहुत तल्लीन था । उसकी तल्लीनता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि उसके सामने से राजा की सवारी निकल गयी और उसे पता ही नहीं चला। ईश्वर पर मन को केन्द्रित करने का अभ्यास करते समय आपकी एकाग्रता इसी प्रकार की होनी चाहिए। ईश्वर — और केवल ईश्वर —का ही विचार आपके मन में होना चाहिए। निस्सन्देह एकाग्रता के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त करने में समय लगता है। सच्ची एकाग्रता के लिए कठिन प्रयास करना पड़ता है।
अभ्यास करते समय मन इधर-उधर भागे, तो भी चिन्ता न करें। पहले इसे दौड़-भाग करने दें। फिर धीरे-धीरे इसे अपने एकाग्रता के विषय पर वापस ले आयें। बार-बार अभ्यास करने से मन अन्ततः हृदय या हृदय में निवास करने वाली परम आत्मा पर केन्द्रित होने लगेगा। शुरू-शुरू में मन ८० बार भागेगा। छह महीने बीतते-बीतते ८० की संख्या घट कर ७० रह जायेगी। एक साल के अन्त में इसकी भाग-दौड़ ५० बार से ज्यादा नहीं होगी। दो वर्ष समाप्त होते-होते यह ३० बार से अधिक नहीं भागेगा और पाँच वर्षों के अन्दर मन दिव्य चेतना में पूर्णतः अवस्थित हो जायेगा। तब आपके चाहने पर मन इधर-उधर नहीं भागेगा। दूसरों के खेतों में घास खाने के लिए भागता-फिरता बैल अब अपनी ही नाँद पर आनन्दपूर्वक चने-बिनौले खाने लगेगा।
एकाग्रता के अभ्यास में अवधान का बहुत महत्त्व है। अवधान की क्षमता विकसित होने पर एकाग्रता का अभ्यास सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन काम-वासना और बेतुकी कामनाओं से भरा हुआ होता है, वह एक क्षण के लिए भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता। उसका मन बन्दर की तरह उछल-कूद मचाता रहता है। यदि आप अपनी एकाग्रता की क्षमता का विकास करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लौकिक कामनाओं और सांसारिक कार्य-कलापों को कम करना होगा। नित्य लगभग दो घण्टे तक मौन रहें। एकाग्रता के विषय की अनुपस्थिति में भी उसका स्पष्ट मानस-दर्शन करने की क्षमता आपमें होनी चाहिए। क्षण-भर में ही उसका मानसिक चित्र आपके मन के परदे पर उभर कर आ जाना चाहिए। यदि आपने एकाग्रता का पर्याप्त अभ्यास किया है, तो आप बिना किसी कठिनाई के यह क्षमता प्राप्त कर लेंगे।
जो साधक सफलतापूर्वक प्रत्याहार (इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाने) का अभ्यास कर लेता है, उसकी एकाग्रता विकसित हो जाती है। अध्यात्म मार्ग पर उसको एक-एक कदम के प्रति जागरूक रहते हुए आगे बढ़ना है। धारणा और ध्यान के भवन का निर्माण यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की आधारशिलाओं पर करें। तभी यह भवन मजबूत बन पायेगा। एकाग्रता के अभ्यास के प्रारम्भिक चरणों में आप घड़ी की टिक-टिक या मोमबत्ती की लौ या अच्छा लगने वाले किसी भी पदार्थ पर मन को केन्द्रित करने का प्रयास करें। इसे स्थूल एकाग्रता कहते हैं। जब तक मन को केन्द्रित करने के लिए कोई आधार न हो, तब तक एकाग्रता सम्भव नहीं है। मन को किसी सुखद विषय पर केन्द्रित किया जा सकता है। मन को जो सुखद न लगे, उस पर उसे (मन को) केन्द्रित कर पाना बहुत कठिन है। मन को शरीर के अन्दर या बाहर के किसी पदार्थ पर या विषय पर केन्द्रित करें। इसे स्थिरतापूर्वक कुछ देर तक केन्द्रित किये रखें। यही 'धारणा' है। यह अभ्यास प्रतिदिन करें। लययोग का भी आधार धारणा ही है।
वेदान्ती साधक मन को आत्मा पर केन्द्रित करने का प्रयत्न करते हैं। हठयोगी और राजयोगी मन को अपने शरीर के छह चक्रों पर केन्द्रित करते हैं। भक्त अपना मन अपने इष्टदेव पर केन्द्रित करते हैं। सभी साधकों के लिए एकाग्रता एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।
जो साधक एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, वे अपना क्रम विकास तेजी से करते हैं। वे कोई भी कार्य अपेक्षाकृत कम समय में अधिक निपुणता से सम्पन्न कर सकते हैं। जो अपने मन को एकाग्र कर लेता है, वह छह घण्टों में पूरा होने वाले कार्य को आधा घण्टे में ही कर लेता है। एकाग्रता का अभ्यास करने से मन शुद्ध होता है, उमड़ती हुई भावनाएँ शान्त होती हैं, चिन्तन-धाराएँ सशक्त बनती हैं तथा विचारों में स्पष्टता आती है। एकाग्रता से भौतिक विकास में भी सहायता मिलती है। एकाग्रता का अभ्यासी दुकान, कार्यालय या कहीं भी अपने काम भली प्रकार निपटा लेता है। जो कार्य उसके लिए पहले अस्पष्ट, धुंधला, कठिन, जटिल, सम्भ्रम उत्पन्न करने वाला प्रतीत होता था, वह अब स्पष्ट, सरल तथा बोधगम्य बन जाता है। मानसिक एकाग्रता की सहायता से सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जिस साधक ने एकाग्रता का नियमित रूप से अभ्यास किया है, उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। परोक्ष-दर्शन, परोक्ष-श्रवण, मूर्छन (mesmerism), सम्मोहन विद्या, परविचार ज्ञान, संगीत, गणित तथा अन्य विज्ञान एकाग्रता पर ही निर्भर रहते हैं। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण तथा संलाग (cohesion) के नियम भौतिक स्तर पर क्रियाशील होते हैं, उसी प्रकार सापेक्षता, साहचर्य तथा संलाग के नियम मानसिक स्तर (या वैचारिक संसार) पर क्रियाशील होते हैं। एकाग्रता का अभ्यास करने वाले साधकों को चाहिए कि वे इन नियमों को भली प्रकार जान और समझ लें।
जब मन किसी पदार्थ के बारे में चिन्तन करता है, तब वह उसके गुणों तथा भागों के बारे में भी सोचता है। जब यह कारण के बारे में सोचता है, तब यह उससे सम्बन्धित कार्य के बारे में भी सोचता है। यदि आप गीता-जैसे धर्मग्रन्थों या अन्य उत्तम पुस्तकों का बार-बार अध्ययन करें, तो हर बार आपको कुछ नये विचार सूझेंगे। एकाग्रता की सहायता से आप इन ग्रन्थों की गहराइयों में उतर पाते हैं। तब आपकी मानसिक चेतना के क्षेत्र में इनके सूक्ष्म गूढ़ अर्थ उभरने लगते हैं। तब आप विचारों के दार्शनिक पक्ष की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल पदार्थों पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। धीरे-धीरे एकाग्रता की पक्की आदत पड़ जायेगी। जैसे ही आप मन को एकाग्र करने के लिए बैठेंगे, अनुकूल मनःस्थिति सहज ही तत्काल बन जायेगी। यदि मन में कामनाएँ हों, तो उन्हें पूरा न करें। जैसे ही वे उत्पन्न हों, उन्हें अस्वीकार कर दें। इस प्रकार धीरे-धीरे उनकी संख्या में कमी आने लगेगी। चित्तवृत्तियाँ भी बहुत कम हो जायेंगी। आपको सभी प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं, अन्धविश्वासों, व्यर्थ कल्पनाओं, कल्पित भयों तथा कुसंस्कारों से मुक्ति पानी है। तभी एकाग्रता के अभ्यास में आप सफल हो सकेंगे।
५. एकाग्रता के व्यावहारिक अभ्यास
(१)
अपने मित्रों से कहें कि वे आपको ताश के पत्ते दिखायें। देखने के तुरन्त बाद आप उनका वर्णन करें। चिड़ी का बादशाह, हुक्म का दहला, ईंट की रानी, पान का गुलाम- जो भी हों, उनके बारे में बतायें।
(२)
किसी पुस्तक के दो-तीन पृष्ठ पढ़ें। फिर पुस्तक बन्द कर दें। अब जो कुछ आपने पढ़ा है, उस पर ध्यान दें। चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाले विचारों का त्याग करें। मन को एक जगह केन्द्रित करें। अब अपने मन से कहें कि वह समान विचारों को एक-साथ रखते हुए उनका वर्गीकरण करे, विचारों के छोटे-छोटे समूह बना ले, फिर उनकी परस्पर तुलना करे। इस प्रकार आप सम्बन्धित विषय का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जल्दी-जल्दी पृष्ठों को उलटने से कोई लाभ नहीं होगा। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कुछ ही घण्टों में पूरी किताब पढ़ डालते हैं। यदि आप उनसे किताब के कुछ अंश सुनाने को कहें, तो यह उनके लिए कठिन हो जायेगा। यदि आप प्रस्तुत विषय पर सावधानीपूर्वक ध्यान दें, तो मन पर बड़ी स्पष्ट और गहरी छाप पड़ती है। छाप गहरी पड़ने पर स्मृति तीव्र होती है।
(३)
ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठें। अपने से एक फुट की दूरी पर एक घड़ी रख लें। घड़ी की टिक-टिक पर मन को धीरे-धीरे एकाग्र करें। जब भी मन इधर-उधर भागने लगे, बार-बार घड़ी की आवाज को सुनने की कोशिश करें। फिर देखें कि आप कितनी देर तक लगातार इस आवाज पर मन को केन्द्रित कर सकते हैं।
(४)
ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठें। आँखें बन्द कर लें। अँगूठों या रुई या मोम से कानों को बन्द कर लें। अनाहत नाद को सुनने की कोशिश करें। आपको विभिन्न प्रकार की आवाजें (बाँसुरी, वायलिन, नक्कारे, तूफान, शंख या घण्टे की आवाज, मधुमक्खी की भिनभिनाहट आदि) सुनायी पड़ेंगी। पहले स्थूल आवाजें सुनने का प्रयत्न करें। एक बार में एक ही आवाज सुनें। मन इधर-उधर भागे, तो उसे स्थूल से सूक्ष्म या सूक्ष्म से स्थूल आवाजों की तरफ ले जा सकते हैं। सामान्यतः दाहिने कान में आवाजें सुनायी पड़ती हैं। कभी-कभी बायें कान में भी सुनायी पड़ती हैं। लेकिन किसी एक कान की आवाजों पर मन को केन्द्रित करें। इससे मन स्थिर हो जायेगा। मन को काबू में रखने का यह एक सरल उपाय है। जैसे साँप बीन की आवाज सुन कर मोहित हो जाता है, उसी प्रकार मन भी इन आवाजों को सुन कर मोहित हो जायेगा।
(4)
अपने सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखें और उसकी लौ पर मन को एकाग्र करें। जब ऐसा करते-करते थक जायें, तब आँखें बन्द कर लें और लौ का मानस-दर्शन करें। प्रारम्भ में आप इस अभ्यास को आधा मिनट तक करें। अपनी रुचि, स्वभाव और क्षमता के अनुसार इस अभ्यास की अवधि को ५ से १० मिनट तक बढ़ायें। जब आप गहन ध्यान की स्थिति में पहुँचेंगे, तब आपको ऋषियों तथा देवताओं के दर्शन होंगे।
(६)
लेट कर चन्द्रमा पर मन को एकाग्र करें। जब-जब मन भागे, इसे वापस चन्द्रमा के बिम्ब पर ले आयें। भावनात्मक स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास बहुत लाभदायक है।
(७)
लेटे-लेटे ऊपर चमकते हुए असंख्य तारों में से किसी एक तारे को क्रम संख्या ६ में वर्णित विधि से अभ्यास करें। चुन लें और क्रम संख्या (६) में वर्णित विधि से अभ्यास करें ।
(८)
एक ऐसी नदी के किनारे बैठें जिसकी लहरें आपस में टकरा कर 'ॐ' का उच्च घोष कर रही हों। इस आवाज पर मन को केन्द्रित करें। जब तक आपकी इच्छा हो, तब तक इसका अभ्यास करें। इस अभ्यास का अनुभव अत्यन्त रोमांचक तथा प्रेरणादायक है।
(९)
विस्तृत नीले आकाश के नीचे लेट कर उस पर मन को एकाग्र करें। इस अभ्यास से आकाश की तरह आपके मन का भी विस्तार होगा। आपको अपने उन्नयन का अनुभव होगा। नीला आकाश आपको आत्मा की असीमता को स्मरण करायेगा ।
(१०)
ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जायें। फिर अनेकानेक अमूर्त गुण (यथा दया) में से किसी एक गुण पर मन को एकाग्र करें। अभ्यास की अवधि का निर्धारण अपनी क्षमता के अनुसार करें।
६. साधना की कुंजी
मन की सभी गतिविधियों और क्रिया-कलापों के प्रति जागरूक होने के बाद अब इसे किसी एक बिन्दु पर केन्द्रित किया जा सकता है। किसी एक पदार्थ, विचार या क्रिया पर मन की शक्ति को एकाग्र करके संकेन्द्रित करना एकाग्रता की प्रक्रिया या एक भाग है। इस संकेन्द्रण से कम-से-कम समय में न्यूनतम प्रयास करके अधिकतम परिणाम प्राप्त होते हैं।
यह नियम मानव-जीवन के प्रत्येक प्रकार के कार्य-कलापों पर लागू होता है। पूरी एकाग्रता और मनोयोग से शल्य-चिकित्सक आपरेशन करता है। जिन-जिन कार्यों में परिशुद्धता (accuracy) नितान्त आवश्यक है (यथा चार्ट या रेखाचित्र या मापचित्र बनाना)। उनमें लगे हुए तकनीशियन, इंजीनियर, वास्तुकार या कलाकार की मनःस्थिति का मुख्य लक्षण गहन तल्लीनता (एकाग्रता) ही होती है। स्विट्जरलैण्ड के उन श्रमिकों की मानसिक स्थिति में भी यही एकाग्रता पायी जाती है, जो घड़ी या अन्य वैज्ञानिक उपकरणों के बारीक पुर्जों का उत्पादन करते हैं।
किसी भी शक्ति को एकाग्र करके उसे किसी एक बिन्दु पर लगा देने से उसका प्रभाव कितना अधिक बढ़ जाता है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं—बाँधों के जल-द्वारों पर जल-प्रवाह की तेजी तथा रेल के बायलर (boiler) से निकलती हुई वाष्प की अन्तश्चालक (impelling) शक्ति। जब सूर्य की किरणें किसी लेन्स (lens) से हो कर गुजरती हैं, तब वे एक अत्यन्त प्रचण्ड आग्नेय किरण में रूपान्तरित हो जाती हैं; इसी प्रकार धारणा के अभ्यास से मन भी एकाग्र हो जाता है। मन तीन बातों के प्रति आकर्षित होता है-ध्वनि, (भौतिक या मानसिक) रूप तथा विचार। योगी अपने मन को प्रणव की गुह्य आन्तरिक ध्वनि पर एकाग्र करके गहन ध्यान की स्थिति में प्रवेश करता है। यही अनाहत नाद है, जो आन्तरिक कोशों के पूर्णतः विशुद्ध हो जाने तथा सामंजस्य स्थापित हो जाने पर सुनायी पड़ता है। यह नाद तब भी सुनायी पड़ता है, जब योगी समस्वरता के साथ किसी मन्त्र का जप करता है तथा अपने मन को लगातार सुनायी पड़ने वाली उसकी ध्वनि पर एकाग्र करता है। अपने मन को केन्द्रित करने के लिए वह इष्टदेव के किसी भी पक्ष के किसी अमूर्त रूप या 'ॐ' के रूप को चुन लेता है। विवेकशील या वेदान्ती साधक किसी उदात्त विचार या सूत्र पर अपने मन को लगातार केन्द्रित किये रहता है।
एकाग्रता की स्थिति में मन शान्त और स्थिर हो जाता है। ध्येय पर मन की वृत्तियों को संकेन्द्रित किया जाता है। दूसरे शब्दों में लक्ष्य पर मन केन्द्रित हो जाता है। मन की उछल-कूद समाप्त हो जाती है। मन में केवल एक ही विचार रहता है। मन उसी एक विचार पर एकाग्र हो जाता है। इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। वे कार्य करना बन्द कर देती हैं। गहन एकाग्रता की स्थिति में शरीर और प्रतिवेश (surroundings) का भान नहीं रहता । जो साधक सफलतापूर्वक एकाग्रता का अभ्यास कर लेता है, वह पलक मारते ही इष्टदेव के रूप का मानसिक दर्शन कर लेता है।
मनोराज्य का कल्पना-लोक में विचरण करना एकाग्रता नहीं है। यह ध्यान भी नहीं है। यह मात्र हवा में मन की छलाँग है। आत्म-विश्लेषण या आत्म-निरीक्षण द्वारा मन की इस आदत के प्रति जागरूक रहें तथा उस पर नियन्त्रण प्राप्त करें।
साधना के विभिन्न मार्गों में ध्यान
ध्यान विभिन्न प्रकार के होते हैं। साधक की रुचि, स्वभाव, क्षमता और उसके मन का स्वभाव - इनके अनुसार ही उसके लिए कोई विशेष प्रकार का ध्यान अनुकूल पड़ता है। भक्त अपने इष्टदेवता का ध्यान करता है। राजयोगी दुःखों, कामनाओं और कर्मों से अप्रभावित एक विशिष्ट पुरुष या ईश्वर का ध्यान करता है। हठयोगी चक्रों और उनके अधिष्ठातृ देवताओं का ध्यान करता है। ज्ञानी अपनी आत्मा का ध्यान करता है। आपको स्वयं यह निर्णय लेना होगा कि आपके लिए कौन-सा ध्यान अनुकूल पड़ता है। यदि आप यह निर्णय स्वयं नहीं ले सकते, तो किसी आत्मसाक्षात्कार प्राप्त गुरु के पास जायें। आपके मन के स्वभाव तथा आपके लिए उपयुक्त ध्यान की पद्धति की जानकारी उन्हें अवश्य ही होगी।
राजयोगी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तथा धारणा का अभ्यास करके विमर्शपूर्वक ध्यान की स्थिति में प्रवेश करता है। भक्त ईश्वर के प्रति अपने पोषित करता हुआ ध्यान की स्थिति में पहुँचता है। वेदान्ती या ज्ञानयोगी श्रवण-मनन शुद्ध द्वारा तथा साधन-चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति तथा मुमुक्षुत्व) से सम्पन्न हो कर प्रेम को इस स्थिति में आता है। हठयोगी प्राणायाम का गहन अभ्यास करके ध्यान करता है।
नियमित ध्यान का अभ्यास करने से अन्तर्प्रज्ञा के द्वार खुलते हैं, मन शान्त और स्थिर होता है, आह्लाद की भावना उत्पन्न होती है और साधक परम पुरुष के सम्पर्क में आता है। ध्यानयोग के मार्ग में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने से मन के भ्रम स्वतः समाप्त हो जाते हैं, अध्यात्म की सीढ़ी का अगला डण्डा अपने-आप दृष्टिगोचर होने लगता है तथा एक गुह्य आन्तरिक स्वर आपका मार्ग-निर्देशन करने लगता है। इस स्वर को ध्यानपूर्वक सुनें ।
जब आप गहन ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं, तब आप अपने शरीर तथा प्रतिवेश से परे हो जाते हैं, आप समचित्तता की स्थिति में पहुँच जाते हैं, आप आसानी से विभ्रान्त नहीं हो सकते, संवेदनाओं का उद्भव तथा विलयन समाप्त हो जाता है, आपका अहं भाव धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है, आप अव्याख्येय तथा वर्णनातीत आनन्द का अनुभव करने लगते हैं। फिर तर्क-वितर्क तथा चिन्तन-मनन की मानसिक प्रक्रियाएँ भी समाप्त हो जाती हैं।
जब गहन ध्यान की स्थिति में आप मौन हो जाते हैं, तब बाह्य संसार तथा आपकी समस्त समस्याएँ समाप्त हो जाती हैं। आप परम शान्ति का अनुभव करने लगते हैं। मौन की स्थिति में ही परम प्रकाश के दर्शन होते हैं तथा आप अक्षय परमानन्द और वास्तविक शक्ति का अनुभव करते हैं। ध्यान की गहराई में पहुँच कर आपके समूचे व्यक्तित्व का कायाकल्प तथा अनुप्राणन हो जाता है।
श्रद्धा योग की शक्ति है। ध्यान से प्राप्त वीर्य (योग-साधना की तत्परता उत्पन्न करने वाले उत्साह के लिए), स्मृति (चिन्तन के लिए), समाधि (मन की एकाग्रता के लिए) तथा प्रज्ञा (ज्ञेय के अपरोक्ष ज्ञान के लिए) असम्प्रज्ञात-समाधि के साधन बन जाते हैं।
दैवी अनुग्रह
सापेक्षता के अवरोध को पार करने के लिए व्यक्ति और परमात्मा के बीच की खाई को समाप्त करने वाली अन्तिम छलाँग ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करके ही लगायी जा सकती है। इस अनुग्रह का अवतरण समर्पण करने से होता है। समर्पण के माध्यम से भक्त वैश्व इच्छा से अपने को एकाकार कर देता है। दैवी अनुग्रह से समर्पण में पूर्णता आती है। इस अनुग्रह के बिना परम ऐक्य सम्भव नहीं है। समर्पण तथा दैवी अनुग्रह परस्पर सम्बन्धित हैं। दैवी अनुग्रह प्राप्त करने के पश्चात् साधना-पथ की बाधाएँ और फन्दे समाप्त हो जाते हैं।
भक्त भाव-समाधि तथा महाभाव की स्थिति में पहुँच जाता है। उसे ईश्वर के प्रगाढ़ आलिंगन का सुख प्राप्त होता है। वह दैवी ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह भगवान् की समस्त दैवी सम्पदा का मालिक बन जाता है। उसे दिव्य चक्षु, दिव्य सूक्ष्म शरीर और दिव्य इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं। वह अपने इष्टदेव में विलय होना नहीं चाहता है। वह उनसे विलग परन्तु उनके सम्मुख ही रह कर दिव्य प्रेम के मधु का पान करते रहना चाहता है। भक्ति के प्रारम्भिक चरणों में प्रेम तथा अनुभव की प्रगाढ़ता हो जाने पर वह अस्थायी रूप से अपने इष्टदेव में विलय भी हो जाता है, यद्यपि यह उसे अभीष्ट नहीं होता। वह ईश्वर का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। प्रारम्भ में वह ईश्वर के सदृश होता है। अन्ततः वह भगवान् से सायुज्य पा लेता है।
समाधि तथा प्रगाढ़ निद्रा
अद्वैत विश्रान्ति तथा प्रगाढ़ निद्रा में अन्तर है। प्रगाढ़ निद्रा में मानसिक क्रियाएँ अज्ञान में विलीन हो जाती हैं, जब कि अद्वैत विश्रान्ति की स्थिति में क्रियाएँ वास्तविक तथा मूर्त ब्रह्म में विलीन होती हैं। प्रगाढ़ निद्रा में सुख अज्ञान से आवृत रहता है; परन्तु अद्वैत विश्रान्ति में प्राप्त होने वाला ब्रह्मानन्द नितान्त अनावृत रहता है।
जिस प्रकार ईंधन के जल चुकने पर आग अपने स्रोत में विलय हो कर शान्त हो जाती है, उसी प्रकार सभी संकल्पों और विचारों के समाप्त हो जाने के बाद मन अपने स्रोत- आत्मा में विलय हो कर शान्त हो जाता है। तभी परम स्वतन्त्रता या कैवल्य की प्राप्ति होती है। एक दिन में सारे विचारों को नष्ट नहीं किया जा सकता। मानसिक वृत्तियों की प्रक्रिया लम्बी और कठिन है। विचारों को समाप्त करने का अभ्यास करते रहें. (भले ही विचार आंशिक रूप से ही समाप्त हुए हों)। आपके प्रारम्भिक प्रयास विचारों को कम करने से सम्बन्धित होने चाहिए।
अपनी आवश्यकताओं और कामनाओं को कम करें। तब विचार भी कम होने लगेंगे। फिर धीरे-धीरे समूचे विचार समूल नष्ट हो जायेंगे। विचार समुद्र की लहरों के समान हैं। उनकी संख्या अनन्त है। प्रारम्भ में उन्हें समाप्त करने के प्रयत्न में शायद आप निराश हो जायें। कुछ विचारों की लहरें उतर जायेंगी, लेकिन कुछ विचार तेज प्रवाह वाली धारा के समान फूट निकलेंगे। जिन विचारों को कभी आपने दमित कर दिया था, कभी दोबारा शिर उठा सकते हैं। अभ्यास करते समय कभी निराश न हों। अवश्य ही वे आपको आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। अन्ततः आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जिस कठिनाई का सामना आप अभी कर रहे हैं, उसका अनुभव प्राचीन काल के सभी योगियों ने किया था।
७. ध्यान
ध्यान दो प्रकार का होता है—स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान । स्थूल ध्यान में साधक भगवान् कृष्ण, भगवान् राम, भगवान् शिव, भगवान् हरि या गायत्री देवी के स्वरूप का ध्यान करता है। सूक्ष्म ध्यान में वह अपने मन की समस्त ऊर्जा को अद्वैत ब्रह्म या आत्मा के विचार पर ही एकाग्र करता है और अन्य रूपों की स्मृतियों तथा विभिन्न आदर्शों की तुलनात्मक विचारणा से अपने को दूर रखता है। केवल ब्रह्म का ही एकमात्र विचार उसके मन में रहता है। किसी आन्तरिक (शरीर के अन्दर) अथवा बाह्य (बाहरी (पदार्थ) बिन्दु या पदार्थ पर मन को केन्द्रित करना एकाग्रता (धारणा) है। इसके बाद की स्थिति ध्यान है।
प्रातः ४ से ६ बजे तक ध्यान का अभ्यास करें। इस अभ्यास के लिए यह समय सर्वोत्तम है; परन्तु आप ध्यान के लिए वह समय भी चुन सकते हैं, जब आपका मन विचार- रहित रहता है तथा आप कम-से-कम विक्षुब्ध रहते हैं। सोने से ठीक पहले भी आप ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। इस समय भी मन शान्त रहता है। रविवार को भी ध्यान का अच्छा अभ्यास कर सकते हैं; क्योंकि अवकाश होने के कारण मन चिन्ताओं से मुक्त रहता है। रविवार को अविराम ध्यान करें। यदि आप केवल दुग्ध-फलाहार का सेवन करें या उपवास करें, तो ध्यान का अभ्यास भली प्रकार कर सकते हैं। सदैव अपने सामान्य बोध का उपयोग करें तथा ध्यानाभ्यास के अच्छे परिणाम प्राप्त करने का प्रयत्न करें।
नैतिक जीवन व्यतीत करके ही गहन ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया जा सकता है। नैतिक जीवन व्यतीत करने से अच्छे-बुरे का विवेक करने की क्षमता प्राप्त होती है। तब आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। जितना ही अधिक नैतिक जीवन आप व्यतीत करेंगे, उतना ही अधिक ध्यान आप कर सकेंगे। तब जन्म-मरण के चक्र से मुक्त बढ़ जायेगी। करने वाली निर्विकल्प-समाधि की स्थिति में प्रवेश करने की भी सम्भावना बढ़ जायेगी ।
नैतिक मूल्यों को अस्वीकार करने वाले मन से ध्यान का अभ्यास करना कमजोर नींव पर मकान बनाने के समान है। ऐसा मकान बन तो जायेगा, परन्तु वह गिरेगा अवश्य । ऐसी स्थिति में आप वर्षों तक भी ध्यान करते रहें, तब भी कोई ठोस परिणाम आपके हाथ नहीं लगेगा। बिना नैतिक आधारशिला के आप नीचे गिर जायेंगे। अतः ध्यान और समाधि में सफलता प्राप्त करने के लिए नैतिक प्रशिक्षण द्वारा मन को शुद्ध करना अत्यन्त आवश्यक है। ध्यान का अभ्यास प्रारम्भ करने से पूर्व आपको आवश्यक सद्द्बोध होना चाहिए, तभी ध्यान में प्रत्याशित सफलता प्राप्त हो सकेगी। ध्यान के अभ्यास में जितना समय लगता है, उससे अधिक समय ध्यान हेतु मन को तैयार करने में लगता है।
मन एक नटखट बालक तथा उछल-कूद मचाने वाले बन्दर की तरह है। इसे अनुशासन में रखने हेतु नित्य ही प्रयत्न किये जाने चाहिए। तब धीरे-धीरे यह नियन्त्रण में आ जायेगा। मन को व्यावहारिक ढंग से प्रशिक्षित करके ही हम उसमें बुरे विचारों को प्रवेश करने से रोक सकते हैं तथा बुरे कार्य करने से बच सकते हैं। बुरे कार्यों तथा विचारों के आवर्तन के कारण जो अन्य बुरे विचार मन में उठने लगते हैं और घटनाओं के चक्र में अपने द्वारा किये गये जो नये कुकर्म जुड़ जाते हैं, उन पर भी नियन्त्रण रखा जा सकता है। मन के व्यावहारिक प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप मन में अच्छे विचार आयेंगे और आप अच्छे कार्य करेंगे; फिर इन्हें स्थायित्व प्रदान करने में भी आपको सरलता होगी।
जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को प्रार्थना, जप, कीर्तन तथा ध्यान रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार समय पर शरीर को भोजन न मिलने पर व्याकुलता होने लगती है, उसी प्रकार कुछ दिनों तक नियमित रूप से जप-प्रार्थना करने के बाद निश्चित समय पर सुबह-शाम प्रार्थना न करने पर मन आकुल व्याकुल होने लगता है। आत्मा को भी निश्चित समय पर भोजन चाहिए। शरीर की अपेक्षा आत्मा को भोजन की अधिक आवश्यकता है। अतः हमें नियमित रूप से प्रार्थना, जप, ध्यान आदि करने चाहिए।
यदि आप किसी पात्र को रोज साफ नहीं करें, तो उसकी चमक जाती रहेगी। पात्र की तरह मन भी है। यदि आप ध्यान का नियमित अभ्यास करके मन को साफ नहीं करते। रहेंगे, तो मन अशुद्ध हो जायेगा। मन का मैल हटाने का सबसे प्रभावकारी उपाय ध्यान ही है। अतः नित्य प्रातः ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।
जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, तो मित्र, कार्यालय, गत दिवस के वार्तालाप आदि बार-बार याद आने और मन में विक्षेप उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सतर्कतापूर्णक मन को इन बाह्य सांसारिक विचारों से हटा कर उसे बार-बार लक्ष्य पर केन्द्रित करना होगा; सांसारिक विचारों की पूर्णतः उपेक्षा करनी होगी; इनसे अपने सभी सम्बन्ध समाप्त करने होंगे; बार-बार अपने से कहना होगा- "मुझे नहीं चाहिए ये विचार; इनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है।" तब धीरे-धीरे ये विचार लुप्त हो जायेंगे।
मस्तिष्क पर बाह्य पदार्थों का प्रभाव निरन्तर पड़ता रहता है। इन्द्रियाँ इन प्रभावों को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। तब मस्तिष्क उद्दीप्त होता है और सम्बन्धित व्यक्ति को उन पदार्थों का बोध हो जाता है। पदार्थों का बोध या चेतना या तो बाह्य उद्दीपन से (इन्द्रियों के माध्यम से) उत्पन्न होती है या आन्तरिक उद्दीपन से (स्मृति के माध्यम से)। इन्द्रियों द्वारा गृहीत प्रत्येक साधारण प्रभाव भी अत्यन्त जटिल अभिवाही उद्दीपन (afferent stimuli) का समूह होता है। अभिवाही उद्दीपन वे उद्दीपन होते हैं जो बाहर से मस्तिष्क की ओर ले जाये जाते हैं। उद्दीपन से मन का अधःस्तर (substratum) जाग्रत हो जाता है। किसी इन्द्रिय द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाये जाने वाले प्रभाव से उत्पन्न मस्तिष्क के अधःस्तर के जागरण के साहचर्य (associations) बड़े जटिल होते हैं।
जब आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हों, तब आपको मस्तिष्क के इस जागरण की उपेक्षा करनी चाहिए। उससे सम्बद्ध सभी प्रकार के अन्यान्य सन्दर्भों और विचारों की स्मृतियों और उनकी तुलनात्मक विचारणा से भी बचने का प्रयत्न करें। मन की समस्त ऊर्जा को ब्रह्म या आत्मा के ही विचार पर केन्द्रित करें। इस विचार की किसी अन्य विचार से तुलना करना अपेक्षित नहीं है।
सभी प्रकार के विचारों से बचने का प्रयत्न करें। इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये जाने वाले प्रभावों की उपेक्षा करें। मन के अधःस्तर पर होने वाली सह-सम्बन्धित क्रिया से उत्पन्न जटिलताओं से अपने को दूर रखें। मन को किसी एक ही विचार पर केन्द्रित करें। मनोभावों की प्रक्रियाओं को रोक दें। अब समग्र मन में केवल एक ही विचार होगा। निष्ठा का भी आविर्भाव हो जायेगा। जिस प्रकार किसी विचार या क्रिया का आवर्तन उस विचार या क्रिया को पूर्ण बनाता है, उसी प्रकार किसी प्रक्रिया या भाव का आवर्तन तन्मयता, एकाग्रता या ध्यान को पूर्णता प्रदान करता है।
अपने मन पर सदैव कड़ी निगाह रखें। हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। मन में चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और कामुकता की लहरों को न उठने दें। ये लहरें ध्यान, शान्ति और प्रज्ञा की शत्रु हैं। उदात्त दिव्य विचारों का मनन करके इनका तुरन्त दी दमन कर दें। अच्छे विचारों का चिन्तन करके, मन्त्रोच्चारण के द्वारा उन्हें मन में रोके रख कर, भगवान् के किसी साकार रूप का ध्यान करके, प्राणायाम का अभ्यास करके, भगवन्नाम-संकीर्तन करके, सत्कार्य करके, बुरे विचारों से उत्पन्न क्लेशों पर मनन करके, मन को सब ओर से हटा करके, विचारों के मूल स्रोतों का विश्लेषण करके, अपने से 'मैं कौन हूँ' से सम्बन्धित प्रश्न बारम्बार पूछ कर या अपनी प्रबल इच्छा-शक्ति का प्रयोग करके बुरे विचारों को नष्ट कर दें। जब आपका मन शुद्ध हो जायेगा, तब बुरे विचार नहीं उठेंगे। जिस प्रकार दुश्मन को उसके शिर उठाते ही, बिलकुल प्रारम्भ में नष्ट कर देना आसान होता है, उसी प्रकार मन में बुरे विचारों के उत्पन्न होते ही उन्हें नष्ट कर देना आसान होता है। बुरे विचारों को अपनी जड़ें न जमाने दें। जैसे ही वे अंकुरित होने लगें, उन्हें नष्ट कर दें।
किसी भी जीव-जन्तु को लोभ, स्वार्थ या क्रोध के वश में हो कर दुःख न पहुँचायें। क्रोध तथा दुर्भावनाओं का त्याग करें। झगड़े तथा उत्तेजना करने वाले वाद-विवादों से बचें। तर्क-वितर्क न करें। यदि आप किसी से लड़ाई कर लें या क्रोध में भर कर बहस करने लगें, तो आप तीन-चार दिनों तक ध्यान नहीं कर सकेंगे; आपके मन का सन्तुलन बिगड़ जायेगा; आपकी ऊर्जा इधर-उधर बह कर नष्ट हो जायेगी। रक्त गरम हो जायेगा; नाड़ियाँ छिन्न-भिन्न हो जायेंगी। आपको सदैव अपना मन शान्त रखने का प्रयत्न करना चाहिए। शान्त मन होगा, तभी ध्यान का अभ्यास सकेगा। शान्त मनआपकी एक मूल्यवान् आध्यात्मिक सम्पत्ति है।
यदि आपको ध्यान के अभ्यास में प्रगति करनी है, तब आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपको सदैव मीठे वचन बोलने चाहिए। आपको प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना है। दूसरों की भावनाओं की पीड़ा पहुँचाने वाले कटु या अशोभनीय वचन आपको नहीं बोलने चाहिए। शब्दों को बोलने से पहले उनके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भली प्रकार सोच लेना चाहिए। आप मितभाषी बनें। यही वाक्-तप है। इससे आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी तथा आपको मानसिक शान्ति एवं आन्तरिक शक्ति प्राप्त होगी।
ध्यान के विविध प्रकार होते हैं। भिन्न-भिन्न साधकों के लिए ध्यान के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार उपयुक्त होते हैं। साधक अपनी रुचि, स्वभाव, क्षमता तथा मन की स्थिति के अनुसार ही ध्यान के किसी-न-किसी प्रकार का चुनाव करता है। भक्त-साधक अपने इष्टदेवता का ध्यान करता है। राजयोगी क्लेशों, कामनाओं और कर्मों से अप्रभावित रहने वाले पुरुष का ध्यान करता है। हठयोगी चक्रों और उनके अधिष्ठातृ देवताओं का ध्यान करता है। ज्ञानयोगी अपनी आत्मा का ध्यान करता है। आपको स्वयं अपने लिए उपयुक्त ध्यान के प्रकार का चयन करना होगा। यदि आप स्वयं ऐसा न कर सकें, तो आत्म-साक्षात्कार प्राप्त किसी गुरु से परामर्श करें। वह आपके मन के स्वभाव को जान सकेंगे तथा आपको ध्यान की सही विधि की जानकारी दे सकेंगे।
जब आप गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब आपको अपने शरीर तथा प्रतिवेश की चेतना नहीं रहती; आपका मन शान्त हो जाता है; आपको बाह्य ध्वनियाँ नहीं सुनायी पड़तीं। संवेदनाओं का उद्भव तथा विलयन समाप्त हो जाता है; अहं भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है; आप वर्णनातीत आनन्द तथा प्रसन्नता का अनुभव करने लगते हैं; तर्क-वितर्क तथा चिन्तन-मनन की प्रक्रियाएँ समाप्त हो जाती हैं।
मन के संवर्धन के लिए मन का प्रशिक्षण अति-आवश्यक है। इसे कई प्रकार से प्रशिक्षित किया जा सकता है। स्मृति को प्रशिक्षित करके, चिन्तन-मनन तथा विवेक का प्रवर्धन करके, 'मैं कौन हूँ' के प्रश्न पर विचार करके मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ध्यान द्वारा स्मृति-संवर्धन का अभ्यास स्मृति को निर्मल बनाता है।
नियमित ध्यानाभ्यास करने वाले योगी का व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है। जो व्यक्ति उसके सम्पर्क में आता है, वह उसकी मृदु वाणी, प्रभावकारी वचनों, आँखों की चमक, देदीप्यमान स्वरूप, स्वस्थ तथा सबल काया, सद्व्यवहार, सद्गुण तथा दिव्य स्वभाव से प्रभावित हो जाता है। जिस प्रकार पानी में डाली गयी नमक की एक डली घुल कर पूरे पानी को नमकीन बना देती है तथा फूल की सुगन्ध आस-पास की हवा को सुगन्धित कर देती है, उसी प्रकार ऐसे योगी की आध्यात्मिक प्रभा व्यक्तियों के मन में प्रवेश करके उनमें व्याप्त हो जाती है। फिर वह लोगों की शान्ति, प्रसन्नता और शक्ति का स्रोत बन जाती है। वे उसके वचनों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मात्र उसके सम्पर्क से ही उनका मन उदात्त होने लगता है।
पूर्ण निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रवेश करने से पूर्व आपको छह अवस्थान पार करने पड़ते हैं। इस अवस्था में रूप-बोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ध्यान और ध्येय-दोनों ही नहीं रह पाते हैं। ध्याता और ध्येय मिल कर एक हो जाते हैं। इस अवस्था में उच्चतम ज्ञान तथा शाश्वत परम शान्ति की प्राप्ति होती है। यही जीवन तथा अस्तित्व का परम ध्येय है। यही जीवन का परमानन्द है। इस स्थिति में आप जीवन्मुक्त हो जाते हैं। दुःख, शोक, भय, सन्देह, भ्रान्तियों के प्रभाव से आप परे हो जाते हैं। आप ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं। बुलबुला अब सागर बन जाता है। सरिता सागर में मिल कर उससे एकाकार हो जाती है। किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाता। आप अनुभव करने लगते हैं— 'मैं ही अमर आत्मा हूँ। समस्त सृष्टि वास्तव में ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।'
एक स्थान है, जहाँ न कोई शब्द सुनायी पड़ता है, न कोई वर्ण दृष्टिगोचर होता है। इस स्थान का नाम है परमधाम या अनामय पद। यहाँ सर्वत्र परम शान्ति और परमानन्द का साम्राज्य है। यहाँ शरीर-बोध नहीं होता। मन को विश्रान्ति प्राप्त होती है। सभी प्रकार की कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं। इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। किसी प्रकार का द्वन्द्व नहीं रहता । क्या आप नीरव ध्यान का अभ्यास करके इस स्थान पर जाना चाहते हैं। यहाँ पवित्र नीरवता का साम्राज्य है। इसी नीरवता में अपने मन को विलीन करके प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इस स्थान में वास किया था। यहाँ ब्रह्म अपनी सहज-सहजात प्रभा से दीप्तिमान होता है।
अपने शरीर तथा अपने प्रतिवेश का विस्मरण कर दें। यह विस्मरण ही सर्वोच्च साधना है। इससे ध्यान में बहुत सहायता मिलती है तथा ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग सरल हो जाता है। ईश्वर का स्मरण करके आप इन सबका विस्मरण कर सकते हैं।
सांसारिक पदार्थों से मन को हटा कर तथा अपने हृदय-कक्ष को निरन्तर प्रकाशित करने वाले भगवान् के चरण-कमलों पर उसे केन्द्रित करके आध्यात्मिक चेतना का अनुभव करें। गहन, नीरव ध्यान का अभ्यास करके अपनी गहराइयों में पैठें। गहरी डुबकी लगायें। सत्-चित्-आनन्द के सागर में स्वच्छन्दता से तैरते रहें। प्रसन्नता की दिव्य सरिता में तैरते रहें। दिव्य चेतना के मूल स्रोत पर अपनी दृष्टि रखें, उसी की ओर बढ़ें और अमृत पान करें। दिव्य आलिंगन की पुलक का अनुभव करें। दिव्य प्रहर्ष का आनन्द उठायें। अभय और अमरता की यही अवस्था है।
प्रतिदिन निश्चित समय पर नियमित रूप से ध्यान करें। तब आप बहुत सरलता से ध्यान की मनःस्थिति में पहुँच जायेंगे। आप जितना ही अधिक ध्यान करेंगे, उतना ही आप अपने आन्तरिक आध्यात्मिक जीवन के अधिक निकट होंगे—जिसमें मन और इन्द्रियाँ अपना खेल नहीं रचा पातीं; आप अपने स्रोत-आत्मा—के बहुत निकट होंगे तथा परमानन्द और शान्ति की लहरें आपको आनन्दित करती रहेंगी। सांसारिक पदार्थ अब आपको आकर्षित नहीं कर पायेंगे। संसार आपके लिए एक लम्बे सपने के समान हो जायेगा ।
सतत, गहन ध्यान के फलस्वरूप आपके अन्दर ज्ञान का प्राकट्य होगा। आप पूर्णतः प्रबुद्ध हो जायेंगे। शरीर का बोध समाप्त हो जायेगा। 'तत् त्वम् असि' महावाक्य का तात्पर्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जायेगा। समस्त प्रकार के द्वित्व, भेद तथा अन्तर समाप्त हो जायेंगे। आप सर्वत्र परमानन्द, प्रकाश और ज्ञान से परिपूर्ण अनन्त असीम आत्मा का दर्शन करने लगेंगे। सचमुच, यह एक दुर्लभ अनुभव होगा। जब यह अनुभव हो रहा हो, तब अर्जुन की तरह भय से काँपने न लगें। निर्भीक बने रहें। आप ऐसे समय अकेले होंगे। न कुछ दिखायी पड़ेगा और न कुछ सुनायी पड़ेगा। इन्द्रियाँ निष्क्रिय हो जायेंगी। सर्वत्र शुद्ध चेतना का ही प्रभाव दृष्टिगोचर होगा।
आप ही आत्मा हैं। आप यह नश्वर शरीर नहीं हैं। इस तुच्छ शरीर के प्रति मोह न रखें। 'मेरा शरीर' – ये शब्द न कहें। शरीर को मात्र 'उपकरण' कह कर सम्बोधित करें।
इस समय सूर्य अस्त हो रहा है। ध्यान के लिए बैठ जायें। अपने अन्दर स्थित त्रिवेणी में अवगाहन करें। मन की वृत्तियों को समेट लें तथा अपनी अन्तरतम गहराइयों में डुबकी लगायें। नीरवता के सागर में विश्राम करें। शाश्वत शान्ति के आनन्द का अनुभवा करें। आपकी जीव-भावना अब समाप्त हो गयी है। समस्त सीमाएँ तिरोहित हो गयी हैं। यदि पुरानी कामनाओं का सर्प फुफकार मारे, तो विवेक के डण्डे तथा वैराग्य की तलवार से उसे मार डालें।
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने तक विवेक और वैराग्य के इन अस्त्रों को अपने साथ कुछ समय तक रखें।
'ॐ' सत्-चित्-आनन्द है। 'ॐ' अनन्त है, शाश्वत है। 'ॐ' का उच्चारण करें, गायन करें, अनुभव करें। 'ॐ' में ही अवस्थित रहें। 'ॐ' का ध्यान करें।
८. ध्यानाभ्यास
किसी एक बिन्दु पर मन को केन्द्रित करना एकाग्रता है। योग-दर्शन में एकाग्रता को धारणा कहते हैं। विचारों की सामूहिकता को एकाग्रता कहते हैं। यदि मन और मनस्तत्त्व किसी एक बिन्दु पर इस प्रकार टिक जायें कि वे न तो अस्थिर रह सकें और न चंचल बन सकें, तो इसे एकाग्रता कहा जायेगा। एकाग्रता के बाद ध्यान की स्थिति आती है। ध्यान में मात्र एक ही विचार निरन्तर बना रहता है।
एकाग्रता की अवस्था में मन इधर-उधर भागता नहीं है। यह अवस्था मन की विचलता को समाप्त करने के लिए होती हैं। इसकी अभिव्यक्ति मानसिक अस्थिरता नहीं, स्थिरता है। प्रसन्न व्यक्ति का मन एकाग्र होता है। जब एकाग्रता होगी, तब मन सहज, स्थिर, एकरस और हर्षित हो जाता है।
ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करें। प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल ध्यानाभ्यास के लिए बैठें। ध्यान का समय तथा स्थान प्रतिदिन एक ही होना चाहिए। सात्त्विक भाव स्वतः ही बिना श्रम किये हुए प्रकट होगा।
ध्यान के लिए नियमितता एक आवश्यक शर्त है। नियमितता से ध्यान के अभ्यास में शीघ्र प्रगति होती है और अमित सफलता प्राप्त होती है। ध्यानाभ्यास के ठोस परिणाम न भी दिखायी पड़ें, तब भी इसे ईमानदारी से धैर्यपूर्वक, दृढतापूर्वक और मन लगा कर करते रहना चाहिए। कुछ समय बाद आपको निस्सन्देह प्रत्याशित सफलता मिलेगी। किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि रुग्णावस्था में भी ध्यान के अभ्यास को रोकना नहीं चाहिए। ध्यान एक उच्च कोटि का टानिक है जिसकी तरंगें सभी प्रकार के रोगों का नाश कर देती हैं। ध्यान से साधक को आध्यात्मिक शक्ति, नव-उत्साह तथा ओजस्विता प्राप्त होती है। ध्यान शरीर और उसकी विभिन्न प्रणालियों का नवीनीकरण कर देता है। ध्यान से शरीर को वास्तविक विश्राम प्राप्त होता है। सात्त्विक भाव को ग्रहण कर पाने के लिए सदैव सतर्क रहें। जैसे ही आप अनुभव करें कि सात्त्विक भाव प्रकट हो रहा है, अपने सारे कार्य रोक कर गम्भीरतापूर्वक ध्यान करने के लिए बैठ जायें।
अहंकार, अभिमान, दर्प, स्वाग्रही राजसिक स्वभाव, चिड़चिड़ापन, दूसरे के कार्यों से अनावश्यक सम्बद्धता, मिथ्याचार — ये सब ध्यान की बाधाएँ हैं। ये शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से मन में छिपी बैठी रहती हैं। समुद्र की अन्तर्धाराओं के समान ये कार्य करती हैं। जिस प्रकार लम्बे समय तक बन्द रहने वाले कमरे की सफाई करने पर धूल ऊपर उठती है, उसी प्रकार योग और ध्यानाभ्यास के अभाव से मन की गन्दगी प्रकट होने लगती है। साधकों को अपना आत्म-विश्लेषण करते रहना चाहिए। उन्हें अपने मन पर सतर्क दृष्टि भी रखनी चाहिए। उनके लिए यह उचित होगा कि वे उपर्युक्त वृत्तियों को उपयुक्त प्रभावकारी उपायों से एक-एक करके हटाते रहें। अहंकार की जड़ें गहरी होती हैं। इसकी शाखाएँ राजसिक मन के समूचे क्षेत्र में फैल जाती हैं। यद्यपि बीच-बीच में अहंकार का प्रभाव कम होता प्रतीत होता है; परन्तु जब भी अवसर मिलता है, यह अपना शिर उठा कर प्रभाव जतलाने का प्रयत्न करता है।
यदि अभ्यासी में छोटी-छोटी बातों को ले कर उत्तेजित हो जाने की आदत है, तो वह ध्यान के अभ्यास में प्रगति नहीं कर सकता। उसे अपना स्वभाव मधुर और सौम्य बना कर अनुकूलनशीलता का गुण अर्जित करना चाहिए, तब उत्तेजित हो जाने की आदत छूट जायेगी। कुछ साधक ऐसे स्वभाव के होते हैं कि यदि उन्हें उनके दुर्गुण बतलाये जायें, तो वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि दुर्गुण बतलाने वाले व्यक्ति ने ईर्ष्यावश उसके दुर्गुणों की कल्पना कर ली है। यह ठीक नहीं है। हमारी अपेक्षा दूसरे व्यक्ति हमारे दुर्गुणों का अधिक सरलता से पता लगा सकते हैं। जिन व्यक्तियों को आत्म-विश्लेषण करने की आदत नहीं है या जो बहिर्मुखी प्रकृति के हैं, वे अपने दोष स्वयं नहीं ढूँढ पाते। अभिमान एक आवरण की भाँति सामने आ जाता है और मानसिक दृष्टि को धुंधला बना देता है। प्रगति करने के लिए साधक को दूसरों के द्वारा इंगित किये गये अपने दुर्गुणों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इंगित करने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उसे अपने दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए; तभी वह ध्यानाभ्यास में प्रगति करते हुए अध्यात्म-क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है।
अपने स्वाग्रही स्वभाव को बदल पाना बहुत कठिन होता है। हम अपने व्यक्तित्व को अनादि काल से निर्मित कर रहे हैं। हमने अपने राजसिक मन को मनमाने ढंग से कार्य करने की छूट दे रखी है। हमारा व्यक्तित्व दुर्नम्य बन गया है। इसे नम्य बनाना कठिन है। स्वाग्रही प्रकृति का व्यक्ति दूसरों पर शासन करना चाहता है। वह दूसरों की युक्तियुक्त, तार्किक तथा तर्कसंगत बातें भी नहीं सुनना चाहता। जिस प्रकार पीलिया के रोगी को सब-कुछ पीला-ही-पीला दिखलायी पड़ता है, उसी प्रकार उसे अपने चारों ओर सब-कुछ गलत-ही-गलत दिखलायी पड़ता है। वह कहने लगता है—“जो कुछ मैं सोचता हूँ, वही ठीक है। दूसरे लोग गलत सोचते हैं।” वह कभी अपनी त्रुटियों को स्वीकार नहीं करता। वह गलत सलत तर्कों द्वारा अपने बेतुके विचारों का ही औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। यदि तर्कों से बात नहीं बनी, तो वह गाली-गलौच और हाथापाई पर उतर आता है। यदि उसे दूसरों से सम्मान नहीं मिला, तो वह क्रोध से आग-बबूला हो जाता है। कोई उसकी चापलूसी करने लगे, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। अपनी बात का औचित्य सिद्ध करने के लिए वह कितने ही झूठ बोल सकता है। जो स्वाग्रही होता है, वह निश्चित ही अपने को सही प्रमाणित करना चाहता है। यह बड़ी खतरनाक आदत है। स्वाग्रही होना और सदैव अपने को सही जतलाने का प्रयत्न करना—ये दो आदतें साधक के ध्यानाभ्यास की प्रगति में तथा उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक हैं। स्वाग्रही व्यक्ति को अपनी मानसिक अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना चाहिए। उसे दूसरों के दृष्टिकोण से सोचने समझने की आदत डालनी चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपने को मिलने वाले मान-सम्मान को कूड़ा-करकट की तरह तथा निन्दा-अपमान को बहुमूल्य आभूषण की तरह समझे।
मनुष्य के लिए अपने को दूसरों की आदतों और स्वभावों के अनुकूल बनाना कठिन होता है। उसके मन में जाति, धर्म, मत आदि के पूर्वाग्रह भरे होते हैं। वह असहिष्णु होता है। वह समझता है कि केवल उसी के विचार ठीक हैं, दूसरों के सभी विचार-मत गलत हैं। दूसरों के दोष ढूँढ़ने में वह बहुत पटु होता है। दूसरों के पुण्य कार्य उसे कभी अच्छे नहीं लगते। वह अपनी क्षमताओं और कार्यों की डींग मारा करता है। यही कारण है कि एक क्षण के लिए भी उसे मानसिक शान्ति नहीं मिलती। वह दूसरों से लम्बे समय तक मित्रता नहीं रख सकता। सभी लोग उसे अपने प्रतिकूल दिखायी पड़ते है। जब साधकों में यही दोष आ जाते हैं, तब उनका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। साधकों को इन दोषों से बचना चाहिए तथा अपने में सहनशीलता, प्रेम आदि सात्त्विक गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए।
योग के मार्ग में बाधाएँ आयेंगी, तो बहुत कठिनाई होगी। तब एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास करना अरुचिकर हो जायेगा। ये बाधाएँ निष्कपट हृदय से प्रार्थना करने, प्रणव या किसी अन्य मन्त्र का जप करने से दूर की जा सकती हैं। ईश्वर कृपा या गुरु-कृपा से भी इनका निवारण किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने भाव-सहित ॐ का जप करने का परामर्श दिया है- “तज्जपस्तदर्थभावनम्' (समाधिपाद: २८) । श्रीं कृष्ण ने गीता में इन बाधाओं से मुक्त होने के लिए कहा है — “मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि—अर्थात् तू अपने विचारों को मुझमें केन्द्रित कर दे, तब तू मेरी कृपा से समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा” (१८ : ५८) ।
यदि कश्मीर में निवास कर रहा कोई साधक उत्तरकाशी में विराजमान अपने गुरु का ध्यान करता है, तो निश्चित ही दोनों में एक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। गुरु तब उसे शक्ति, शान्ति, प्रसन्नता और परमानन्द प्रदान करता है। तब साधक शक्तिशाली चुम्बकीय तरंगों में अवगाहन करने लगता है। आध्यात्मिक विद्युत् का स्रोत एक पात्र से दूसरे पात्र की ओर प्रवाहित होने लगता है। तब शिष्य (गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के अनुपात में गुरु से शक्ति प्राप्त करता है। जितनी ही अधिक श्रद्धा होगी, उतनी ही अधिक शक्ति वह प्राप्त करेगा। जब शिष्य पूरे मन से गुरु का ध्यान करता है, तब गुरु सचमुच यह अनुभव करता है कि शिष्य की ओर से उदात्त विचारों की तरंगें प्रवाहित हो रही हैं और उसके (गुरु के) हृदय को छू रही हैं। उस स्थिति में आन्तरिक सूक्ष्म दृष्टि से शिष्य और गुरु के बीच प्रकाश की एक चमकदार रेखा देखी जा सकती है। यह रेखा चित्त के सागर में सात्त्विक विचारों की तरंगों की गति से निर्मित होती है।
यदि आप उच्चतर आध्यात्मिक स्तर से संसार पर दृष्टिपात करें, तो आपको संसार का एक अत्यन्त स्पष्ट दृश्य दिखायी पड़ेगा। तब परम वैश्व चेतना की स्थिति में आपको समस्त संसार का ज्ञान हो जायेगा। भगवान् कृष्ण के विश्व-रूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन ने कहा :
"धृतराष्ट्र के पुत्र (राजाओं के समुदाय सहित) आपके विकराल जबड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए शिरों सहित आपके दाँतों के बीच में लगे हुए दीखते हैं। आप सम्पूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करतेरहे हैं। हे विष्णो! आपका उग्र प्रकाश सम्पूर्ण जगत् को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है" (११ २७, ३० ) ।
जिस प्रकार किसी छोटी झील में मछलियाँ और जल के छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े इधर-उधर घूमते हैं, जिस प्रकार चींटियाँ दीवाल पर चलती हैं; उसी प्रकार ये छोटे-छोटे मानव भगवान् के शरीर के अन्दर इधर-उधर घूमा करते है। यह दृश्य अत्यन्त रोमांचक तथा विस्मयकारी है। जिस प्रकार ताजे खून की एक बूँद में अनेक श्वेत कोशिकाएँ (leucocytes) तथा लोहित कणिकाएँ (red corpuscles) घूमा करती हैं, उसी प्रकार सहस्रों अविकसित आत्माएँ अनगिनत कामनाएँ लिये हुए इधर-उधर फिरती रहती हैं। अज्ञानी, अविकसित मानवों की भीड़ में आपको बहुत थोड़े व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो पूर्णतः विकसित, जीवन्मुक्त, ज्ञानी या योगी हैं। जिस प्रकार रात के अँधेरे में एक प्रकाश-गृह स्टीमर के कैप्टन का मार्ग-निर्देशन करता है, उसी प्रकार संसार के विभिन्न भागों में निवास करने वाले ये महान् व्यक्ति दिव्य ज्योति की तरह अज्ञानी आत्माओं—साधकों का मार्ग-निर्देशन करते हैं। कुछ ऐसे भी विकासशील, अर्ध-विकसित साधक हैं जिनसे निकलने वाली दिव्य ज्वाला बहुत बड़ी नहीं होती। वे अमावस्या की रात्रि में तारकों की तरह चमकते हैं। यह दृश्य अत्यन्त आश्चर्यजनक है। अन्तर्प्रज्ञा की नवीन दृष्टि से देखने पर यह आन्तरिक यौगिक दृश्य अत्यन्त भव्य लगता है।
तैलधारा (की निरन्तरता) के समान एकमात्र ब्रह्म के विचार को निरन्तर बनाये रखना योग की भाषा में ध्यान कहलाता है। ज्ञानी इसे निदिध्यासन कहते हैं। भक्तों की दृष्टि में यह भजन है।
किसी धधकती हुई भट्ठी में लोहे का टुकड़ा डाल दें। यह आग के रंग के समान लाल हो जायेगा। यदि आप चाहें कि इसका लाल रंग बना रहे, तब इसे लगातार आग में ही रखना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आप मन को ब्रह्मज्ञान की अग्नि से आवेशित रखना चाहते हैं, तो सतत तथा गहन ध्यान के द्वारा आपको इसे निरन्तर ब्रह्मज्ञान की अग्नि के सम्पर्क में रखना पड़ेगा, आपको ब्रह्म-चेतना का निरन्तर प्रवाह बनाये रखना होगा; तब आप सहज अवस्था में प्रवेश करेंगे।
ध्यान एक प्रभावकारी टानिक के समान है। यह मन और नाड़ियों को बल प्रदान करता है। इसके पावन स्पन्दन शरीर की समस्त कोशिकाओं को अनुप्राणित कर देते हैं। ये शरीर को रोगमुक्त भी करते हैं। जो साधक ध्यान करते हैं, उन्हें दवाओं पर अपना धन व्यय नहीं करना पड़ता। ध्यान के समय जो सशक्त शामक तरंगें उठती हैं, वे मन, नाड़ियों, कोशिकाओं और अवयवों पर बहुत हितकर प्रभाव डालती हैं; तब दिव्य ऊर्जा तैलधारावत् भगवान् के चरणों से साधकों की ओर निर्बाध प्रवाहित होने लगती है।
यदि आप आधा घण्टे तक ध्यान करें, तो इसके प्रभाव से प्राप्त शान्ति तथा आध्यात्मिक बल की सहायता ले कर आप एक सप्ताह तक जीवन की समस्याओं से जूझते रह सकते हैं । ध्यान का ऐसा मंगलकारी प्रभाव होता है। अपने दैनिक जीवन में आपको विभिन्न स्वभावों के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना होता है। ध्यान से आपकी ऐसी क्षमता प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से आप उनके साथ भली प्रकार निर्वा सकेंगे।
गीता में आपको ये शब्द बार-बार पढ़ने को मिलेंगे- 'अनन्य चेतस्', 'मच्चित', 'नित्ययुक्त', 'मन्मनस्', 'एकाग्रमन', 'सर्वभाव' ये शब्द यह द्योतित करते हैं कि आपको अपना शतप्रतिशत मन सम्पूर्ण मन भगवान् को अर्पित करना होगा। इसके बाद ही आत्म-साक्षात्कार सम्भव हो सकेगा। यदि मन की एक भी वृत्ति ईश्वरोन्मुख नहीं हो पायी, तो आत्म-साक्षात्कार असम्भव हो जायेगा।
शान्त हो जायें। अपने को जानें 'उसे' (ब्रह्म को) जानें। उसमें (ब्रह्म में) मन को विलीन कर दें। सत्य नितान्त शुद्ध और सरल तत्त्व है।
आसन का अभ्यास करके शरीर को स्थिर करें। बन्धों और मुद्राओं से शरीर को सुदृढ़ बनायें। प्राणायाम करें और शरीर को हलका बनने दें। नाड़ी शुद्धि करके मन में स्थिरता लायें। जब इतना हो जाये, तब ब्रह्म पर मन को केन्द्रित करें, तब ध्यान की प्रक्रिया अनवरत और सुगम हो जायेगी।
गंगा या नर्मदा नदियों के किनारे, हिमालय पर, फुलवारियों या मन्दिरों में ध्यान या एकाग्रता का अभ्यास करते समय मन का उन्नयन होता है। अतः साधक को ऐसे में स्थानों का चुनाव करना चाहिए।
एकान्त तथा ठण्ढे स्थान, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, बदरीनारायण जैसे स्थानों में पाये जाने वाले आध्यात्मिक स्पन्दन तथा शीतोष्ण जलवायु—ये मन की एकाग्रता के लिए अपरिहार्य आवश्यकताएँ हैं। जिस प्रकार नमक पानी में घुल जाता है, उसी प्रकार ध्यान की अवस्था में सात्त्विक मन भी अपने अधिष्ठान — ब्रह्म में विलीन हो जाता है।
ध्यानाभ्यास के प्रारम्भिक चरणों में अभ्यास के लिए बैठने के बाद शुरू-शुरू में दश मिनट तक सुन्दर-सुन्दर श्लोकों और स्तोत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार मन का उन्नयन होगा। तब मन को सांसारिक पदार्थों से हटा पाना सरल हो जायेगा। अब मन को बार-बार प्रयत्न करके एक ही विचार पर केन्द्रित करें। तब निष्ठा का आविर्भाव होगा। ध्यान का अभ्यास प्रारम्भ करने से पूर्व ईश्वर की मूर्ति या उसका मानसिक रूप आपके समक्ष अवश्य होना चाहिए।
जब आप खुली आँखों से भगवान् कृष्ण की मूर्ति देखते हैं और उस पर मन को केन्द्रित करते हैं, तब यह स्थूल ध्यान कहलाता है। जब आप आँखें बन्द करके भगवान् कृष्ण की मूर्ति का चिन्तन करते हैं, तब भी यह स्थूल ध्यान है; परन्तु किंचित् अमूर्त भी है। जब आप असीम अमूर्त प्रकाश का चिन्तन करते हैं, तब ध्यान और भी अधिक अमूर्त हो जाता है। पहले दो उदाहरण सगुण ध्यान के हैं और तीसरा उदाहरण है निर्गुण ध्यान का । प्रारम्भ में निर्गुण ध्यान में भी एक रूप — अमूर्त रूप —रहता है, जिस पर मन केन्द्रित किया जाता है। बाद में यह रूप लुप्त हो जाता है तथा ध्याता और ध्यान एक हो जाते हैं। ध्यान का स्रोत मन है।
अपने चरित्र पर चिन्तन-मनन करें। अपने चरित्र के कुछ दोष ढूँढ़ निकालें। फिर उन दोषों के विपरीत भावात्मक गुणों का ध्यान करें। मान लें कि आपमें चिड़चिड़ाहट का दुर्गुण है। इसका विपरीत भावात्मक गुण है सहन-शक्ति । नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातःकाल चार बजे सिद्धासन या पद्मासन में किसी एकान्त कक्ष में बैठें। सहन-शक्ति, उसकी महत्ता, उत्तेजित होने पर सहनशील बने रहने की अभ्यास- विधि— इन बातों पर मनन करें। एक दिन में एक ही बात पर मनन करें और भली प्रकार मनन करें। मन इधर-उधर भागने लगे, तो उसे फिर विषय पर वापस ले आयें। ऐसा सोचें कि आप पूर्णतः सहनशील बन गये हैं; आप सहन-शक्ति के साकार विग्रह ही है। अन्त में यह प्रतिज्ञा करें - "सहनशीलता ही मेरा यथार्थ स्वभाव है। में आज से ही अपने कार्यों और व्यवहारों में इस गुण को परिलक्षित होने दूंगा।"
प्रारम्भ में आपको अपने स्वभाव में कोई विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपकी चिड़चिड़ाहट वैसी की वैसी आपके स्वभाव का एक अंग बनी हुई है। परन्तु आप नियमित रूप से प्रत्येक सुबह उपर्युक्त अभ्यास करते रहें। इसका परिणाम यह होगा कि जैसे ही आप कोई उत्तेजनशील वस्तु देखेंगे, स्वतः ही एक विचार आपके मन में उठेगा आपको सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। अभ्यास करते जायें। धीरे-धीरे उत्तेजनकारी वस्तु देखने पर सहनशील बनने का विचार उठने के साथ-साथ चिड़चिड़ाहट की बाह्य अभिव्यक्ति नियन्त्रित होती जायेगी। अभ्यास करना बन्द न करें। चिड़चिड़ाहट का आवेश धीरे-धीरे क्षीण होता जायेगा। अन्ततः यह बिलकुल समाप्त हो जायेगा उत्तेजनकारी परिस्थितियों में भी सहनशील बने रहना आपका सामान्य स्वभाव बन जायेगा। इसी प्रकार आप सहानुभूति, आत्म-संयम, शुचिता, विनम्रता, परोपकारिता, भद्रता और उदारता के गुणों का भी विकास कर सकते हैं।
ये मन की क्रियाएँ होती हैं, जिन्हें कर्म कहा जाता है। मन का मोहभंग होने से ही वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। जो अपने को मन के उतार-चढ़ावों से मुक्त कर लेते हैं, वे परम निष्ठा से सम्पन्न हो जाते हैं। समस्त अशुद्धताओं से मुक्त हो जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। तब वह बिलकुल शान्त हो जाता है तथा सांसारिक विभ्रम तुरन्त ही नष्ट हो जाते हैं।
जब शुद्ध मन को ईश्वर पर केन्द्रित किया जाता है, तभी वास्तविक शान्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। आपका जन्म इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। राग और मोह के ही कारण आप बाह्य पदार्थों के प्रति आकर्षित होते हैं। हृदय में ईश्वर का ध्यान करें। हृदय की गहराइयों में पैठने का प्रयत्न करें। वहीं तो दिव्य ज्योति—ज्योतियों की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। इस गहराई में छलांग लगा कर उसके साथ एकाकार हो जायें।
यदि आप किसी कुत्ते के सामने रोटी रख कर उसे किसी दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखने दें, तो वह उसे (प्रतिबिम्ब को) देख-देख कर भौंकने लगेगा। वह यह सोचने लगेगा कि दर्पण वाला कुत्ता उससे भिन्न कोई अन्य कुत्ता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने मन रूपी दर्पण की सहायता से अन्य व्यक्तियों में अपना ही प्रतिबिम्ब देखता है, परन्तु मूर्खतावश यह समझने लगता है कि वे सब उससे भिन्न हैं। इसी कारण वह उनसे घृणा और द्वेष करने लगता है।
आग जलाने के लिए पहले घास-पात, कागज के टुकड़े और छोटी-छोटी लकड़ियाँ जमा करते हैं। आग जल जाती है। लेकिन यह आग शीघ्र ही बुझ जाती है। तब आप फूँकनी से फूँक लगाते हैं और आग जलने लगती है। अब आग पहले से अधिक प्रचण्ड हो जाती है, जिसे आप प्रयत्न करके भी नहीं बुझा सकते। उसी प्रकार ध्यानाभ्यास के प्रारम्भिक चरणों में नये अभ्यासी ध्यान करते-करते फिर अपने छोटे-से संसार के धरातल पर उतर आते हैं। उन्हें बार-बार अपने मन का उन्नयन करके उसे लक्ष्य पर केन्द्रित करना होगा। जब ध्यान गहन और स्थिर हो जायेगा, तब अन्ततः वे ईश्वर में संस्थित हो जायेंगे। तब ध्यान हमारी सहज आदतों का एक अंग बन जायेगा ।
९. ध्यानाभ्यास के फल
नये साधकों को कुछ महत्त्वपूर्ण वैदिक मन्त्रों को याद रखना चाहिए। तभी उनके सन्देह दूर हो सकेंगे, तभी वे साधना के सही मार्ग से आगे बढ़ सकेंगे। ये मन्त्र है
१. सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् -आरम्भ में एकमात्र अद्वितीय सत् ही था। (छान्दोग्योपनिषद् ६, २, १)
२. ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् - यह जगत् पहले एकमात्र परमात्मा ही था (ऐतरेयोपनिषद् १, १, १)
३. तदेतद्ब्रह्मापूर्वमपरमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू: - यह ब्रह्म अपूर्व (कारण-रहित) अनपर (कार्य-रहित) है। यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है। (बृहदारण्यकोपनिषद् २, ५, १९)
०४. आनन्दरूपममृतं यद् विभाति — जो आनन्दस्वरूप अविनाशी परब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित हैं। (मुण्डकोपनिषद् २, २, ७)
अपने वर्तमान से ही सम्बन्ध रखें। भूत और भविष्य की चिन्ता न करें। तभी आपको वास्तविक प्रसन्नता मिलेगी। आप चिन्ताओं से मुक्त हो जायेंगे। आप दीर्घजीवी होंगे। कठिन परिश्रम करके अपने संकल्पों का नाश करें। सच्चिदानन्द ब्रह्म का अनवरत ध्यान करें तथा परम निष्कल्मष पद प्राप्त करें। प्रबुद्धावस्था में आप ब्रह्मानन्द के सागर में निमन रहें, यह कामना है।
अनवरत अभ्यास किये बिना आत्म-साक्षात्कार होना कठिन है। जो सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो कर अमरता प्राप्त करना चाहता है, उसे दीर्घ काल तक आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए।
अद्वैत ब्रह्म ही साधकों के लिए एकमात्र एकान्त स्थान है, जहाँ वे निवास कर सकते हैं। वहाँ न कोई ध्वनि सुनायी पड़ती है और न कोई रंग दिखायी पड़ता है। वहाँ किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं है। ध्यानाभ्यास के प्रारम्भ में ब्रह्म ही साधक का एकमात्र सखा है। गहन ध्यान की अवस्था में जब आप 'वह' बन जाते हैं, तब मात्र आपका ही अस्तित्व होता है (शिव केवलोऽहम् )।
आत्मा समस्त ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा स्रोत आत्मा का ध्यान ऊर्जा, शक्ति और बल में वृद्धि करने का एक सक्रिय उपाय है। यदि आप एक क्षण के लिए भी सर्वव्यापक अमर सच्चिदानन्द आत्मा (अथवा ब्रह्म) का चिन्तन कर लें, तो यह प्रयाग स्थित त्रिवेणी में १००८ बार अवगाहन करने के समान होगा। यही वास्तविक मानसिक अवगाहन है। ज्ञान तथा प्रज्ञा में किये गये इस आन्तरिक अवगाहन की तुलना में शरीर से किये गये स्नान का कोई महत्व नहीं है।
ज्ञान, सन्तोष, शान्ति, प्रसन्नता और समदृष्टि के पुष्पों से ब्रह्म या आत्मा की आराधना करें। यही वास्तविक आराधना है। गुलाब चमेली के फूल, अगरबत्ती और मिठाई तथा फलों के भोग से अज्ञानी ही पूजा करते हैं। ज्ञान-सन्तोष के पुष्पों से की गयी आराधना के समक्ष फूल-चन्दन से की गयी पूजा का कोई मूल्य नहीं है।
अपने अन्तरतम में निवास करने वाले शाश्वत अविनाशी शुद्ध-बुद्ध आत्मा से स्थापित करें सदैव यह सोधें और अनुभव करें" ही शुद्ध 1 मात्र यही विचार सारे कष्टों और सन्देहों का निवारण कर देगा। मन आपको धोखा दे चाहता है। वह चोरों की तरह यात में बैठा रहता है। उपर्युक्त विचार से मन की दुरभिम विफल कर दें।
१०. 'ॐ' का ध्यान
अपने ध्यान कक्ष में प्रवेश करें। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या सुखासन में बैठे अपनी पेशियों को ढीला करें और उनका तनाव समाप्त करें। आँखें बन्द कर भूमध्यबिन्दु पर दृष्टि केन्द्रित करें ब्रह्म-भावना से 'ॐ' का मानसिक उच्चारण करें - यह भावना रखना ध्यान में सफलता प्राप्त करने की एक अनिवार्य तथा अत्यन्त महत्त्वपू शर्त है। अपने चेतन मन को शान्त करें।
निम्नांकित वाक्यों का मानसिक उच्चारण करें। साथ ही साथ इनसे ध्वनित वाले अर्थों की अनुभूति भी करें :
मैं ही सर्वव्यापी प्रकाश का सागर हूँ .... ॐ ॐ ॐ
मैं ही अनन्तता हूँ .... ॐ ॐ ॐ
मैं ही असीम प्रकाश हूँ . .... ॐ ॐ ॐ
मैं ही व्यापक, परिपूर्ण ज्योतिर्मय ब्रह्म हूँ .... .... ॐ ॐ ॐ
मैं ही सर्वशक्तिमान् है .... ॐ ॐ ॐ
मैं ही सर्वज्ञ हूँ .... ॐ ॐ ॐ
मैं ही पूर्ण परमानन्द हूँ ........ .... ॐ ॐ ॐ
मैं ही सच्चिदानन्द हूँ. .... ॐ ॐ ॐ
मैं ही पूर्ण शुचिता हूँ .... ॐ ॐ ॐ
मैं ही पूर्ण गौरव हूँ .... ॐ ॐ ॐ
इस प्रकार से उच्चारण करने से सभी उपाधियों का परिष्कार हो जायेगा। समस्त ग्रन्थियाँ उच्छेदित हो जायेंगी। सभी प्रकार के आवरण समाप्त हो जायेंगे। पंचकोश- अध्यास भी दूर हो जायेगा। आप सच्चिदानन्द की स्थिति में प्रवेश करेंगे। आप परम ज्ञान, परमानन्द तथा आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आप अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। "ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति ।" निःसन्देह आप शुद्ध सच्चिदानन्द व्यापक परिपूर्ण ब्रह्म हो जायेंगे।
आत्म-दर्शन करना बिलकुल कठिन नहीं है। पलक झपकाने में, फूल की पंखुड़ी भेदने में या अन्न के दाने को बरतन पर से लुढ़कने में जो समय लगता है, उससे भी कम समय में आत्म-दर्शन हो सकता है; परन्तु आपको गम्भीरतापूर्वक अनवरत गहन अभ्यास करना होगा। दो-तीन वर्षों के अन्दर आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी।
आजकल अनेक वाचाल ब्रह्म दिखायी पड़ जाते हैं, ज्यादा बातें करने से कोई ब्रह्म नहीं बन जाता। अनवरत गहन और गम्भीर साधना करके ही ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हो सकता है। तब ब्रह्म उतना ही स्थूल दिखायी पड़ता है, जितनी कमरे की दीवाल। उसका उसी प्रकार अनुभव होता है, जिस प्रकार मेज-जैसे किसी मूर्त पदार्थ का होता है।
११. ध्यानसम्बन्धी निर्देश
मोक्षप्रिय ने कहा — गुरुदेव ! मुझे ध्यान से सम्बन्धित निर्देश दें। मैं ब्राह्ममुहूर्त में प्रातः चार बजे से ही ध्यान का अभ्यास करने का प्रयत्न करता हूँ, फिर भी मेरा मन भटकने लगता है।
गुरुदेव ने उत्तर दिया- मोक्षप्रिय ! मन को एकाग्र करके ध्यान से भरी बातें सुनें । "ध्यानं निर्विषयं मनः " मन को ऐन्द्रिय विषयों से मुक्त करना ही ध्यान है। ध्यान की अवस्था में मन ईश्वर —–तथा केवल ईश्वर — पर केन्द्रित रहता है।
अचानक ही ध्यान या समाधि की गहराई में छलाँग लगाना सम्भव नहीं है। ऐसा करने से हाथ-पैर टूट जायेंगे। तीसरी कक्षा का विद्यार्थी सापेक्षवाद के सिद्धान्त या उच्च गणित की बातें कैसे समझ सकता है?
निःस्वार्थ सेवा, भगवन्नाम-जप, प्राणायाम आदि द्वारा पहले अपने को शुद्ध करें। सदाचारी बनें। नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनें। तभी ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं।
एकाग्रता (धारणा) के बाद ध्यान की तथा ध्यान के बाद समाधि की अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है।
हे मित्र हे मोक्षप्रिय! प्रारम्भ में स्थूल मन को ध्यान के लिए स्थूल पदार्थ की आवश्यकता होती है। शुरू-शुरू में किसी स्थूल स्वरूप जैसे हाथ में वंशी लिये हुए भगवान् कृष्ण या भगवान् ईसा या भगवान् बुद्ध के स्वरूप पर ध्यान करना बहुत आवश्यक होता है। यह सगुण ब्रह्म का ध्यान है।
ईश्वर के स्वरूप पर ध्यान करते समय उसके गुणों-जैसे सर्वव्यापिता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता, शुचिता, पूर्णता के बारे में सोचें धीरे-धीरे मन शुद्ध निर्गुण ब्रह्म निराकार और निर्गुण ध्यान के लिए तैयार तथा अनुशासित हो जायेगा।
ध्यान की स्थिति एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने में नहीं आती। आपको दीर्घ अवधि तक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। धैर्य तथा दृढ़ता बनाये रखें। सावधान तथा परिश्रमी बने रहें। सब प्रकार की कामना-वासनाओं से मुक्त हो जायें। पूर्ण अनासक्त भाव से आत्म-साक्षात्कार की तीव्र अभिलाषा रखें। धीरे-धीरे आप गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने लगेंगे।
हे मोक्षप्रिय! प्रयत्न करें और प्रयत्न करते जायें। कठिन परिश्रम करें। ध्यान करें, ध्यान करें, ध्यान करें। अन्त में अवश्य सफलता मिलेगी। हे आध्यात्मिक वीर साधक! मेरे शब्दों पर ध्यान दें।
१२. ध्यान में बाधाएँ
मोक्षप्रिय ने कहा—भगवन् ! कृपा करके बतायें कि ध्यान का अभ्यास करते समय कौन-कौन सी बाधाएँ आ उपस्थित होती हैं ?
गुरुदेव ने उत्तर दिया- मोक्षप्रिय! मन लगा कर सुनें ध्यान की मुख्य बाधाएं दे हैं-लय (निद्रा), विक्षेप (मन की चंचलता ), कषाय (वासना), रसास्वाद (सविकल्प समाधि का परमानन्द), ब्रह्मचर्य का अभाव, आध्यात्मिक दर्प, आलस्य, रोग, सांसारिक व्यक्तियों की संगति, बहुत अधिक भोजन करना, बहुत अधिक काम करना, दूसरों के साथ बहुत अधिक घुलना मिलना, स्वाग्राही होना तथा राजसिक स्वभाव ।
प्राणायाम, आसन और हलके भोजन की सहायता से निद्रा पर विजय प्राप्त करें। प्राणायाम, जप, उपासना, त्राटक आदि से विशेष दूर करें।
वैराग्य, विवेक, वैराग्य से सम्बन्धित पुस्तकों के स्वाध्याय, ध्यान, परिपृच्छा आदि से कषाय दूर करें।
रसास्वाद वह परमानन्द है जो निम्नस्तरीय सविकल्प-समाधि की अवस्था में रहते हुए प्राप्त होता है। यह परमानन्द भी ध्यान की एक बाधा है। इसका कारण यह है कि योगी इस अवास्तविक सन्तोष को ही सब कुछ मान बैठता है। वह समझने लगता है कि वह उच्चतम निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रवेश कर गया है। वह साधना करना बन्द कर देता है और ध्यान की वह उच्चतम अवस्था तक पहुँचने के लिए प्रयत्न करना छोड़ देता है। रसास्वाद से ऊपर उठें, प्रयत्न करें तथा निर्विकल्प समाधि की स्थिति में प्रवेश कर जायें।
ब्रह्मचर्य का पालन न करने से मन अशुद्ध हो जाता है। सांसारिक जीवन की अवधि बढ़ जाती है और कामुक वासनाओं की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। अतः अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करें।
जब साधक आध्यात्मिक विकास करने लगता है, तब उसमें आध्यात्मिक दर्प की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह अपने को गृहस्थों से श्रेष्ठ समझने लगता है। माया तरह-तरह के रूप धारण करके आती है। आत्म-विश्लेषण तथा स्व-अन्वेषण से इस दर्प को नष्ट कर दें।
आलस्य एक दूसरी बाधा है। आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। नित्य दो घण्टे तक पूर्ण उत्साह से निःस्वार्थ सेवा करें। दौड़ें। कुएँ से पानी निकालें। पत्थर ढोयें । आलस्य दूर हो जायेगा।
स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों का पालन करें। नियमित रूप से व्यायाम, आसन, प्राणायाम करें। खाने-पीने में मिताचारी रहें। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
यौन विषयों तथा सांसारिक समस्याओं में रुचि लेने वाले व्यक्तियों का संग न करें।
बहुत अधिक कार्य न करें, अन्यथा आप थक जायेंगे और आप ध्यान न कर सकेंगे। लोगों से बहुत अधिक मिलना-जुलना ठीक नहीं है। इससे राग-द्वेष की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। मन भी अशान्त हो जाता है।
नम्रता, परिपृच्छा, चिन्तन-मनन तथा ध्यान से अपने स्वाग्रही राजसिक स्वभाव को नष्ट कर दें। सावधान रहें। मन को सात्विक विचारों से भर दें।
हे मोक्षप्रिय एक-एक कर बाधाओं को दूर कर दें। अध्यात्म मार्ग पर निर्भीकता से चलते रहे तथा शीघ्र ही अपने गन्तव्य पर पहुंच कर अपना लक्ष्य प्राप्त करें।
१३. ध्यान के अनुभव
मोक्षप्रिय ने कहा- गुरु महाराज! ध्यान के कौन-कौन से अनुभव होते हैं।
गुरुदेव ने उत्तर दिया- सभी साधकों के अनुभव एक से नहीं होते। कौन-सी साधना कर रहा है तथा वह किस योग का अभ्यास कर रहा है, इसके ही उसे अनुभव होते हैं; परन्तु निर्विकल्प समाधि के अनुभव सभी को एक ही प्रकार के अनुनय होते हैं।
हठयोगियों तथा लययोगियों को अनाहत नाद सुनायी पड़ता है। यह नाद की। स्थूल और कभी सूक्ष्म होता है। कभी घण्टियों, ढोल, बाँसुरी अथवा वीणा की आवाज सुनायी पड़ती है, कभी मेघ गर्जन, मृदंग आदि की आवाज सुनायी पड़ती है।
कुछ राजयोगियों को ध्यान करते समय भ्रूमध्य-बिन्दु (आज्ञाचक्र) में चमकीला प्रकाश दिखायी पड़ता है। यह सूर्य, चन्द्रमा, तारकों अथवा स्फुलिंग के प्रकाश की होता है। कभी-कभी हरे, नीले, लाल आदि रंगों का प्रकाश भी दिखायी पड़ता है।
कभी-कभी साधकों को नदियों, पहाड़ों तथा नीले आकाश के दृश्य दिखायी पड़ते हैं। कभी-कभी ध्यान में ऋषि-मुनियों के दर्शन हो जाते हैं। कभी-कभी अपना ही चेहरा दिखायी पड़ने लगता है।
उन्नत योगियों को वैश्व चेतना के दर्शन होते हैं। यह एक असाधारण अनुभव - होता है।
कुछ साधक हवा में तैरते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर उनके स्थूल शरीर से अलग हो जाता है और वह सूक्ष्म लोकों की यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है।
भक्तों को अपने- अपने इष्टदेवों के दर्शन होते हैं।
उन्नत भक्त ब्रह्मलोक, वैकुण्ठ तथा कैलास को जाते हैं।
ज्ञानयोगी तम, तन्द्रा और मोह की स्थितियों से हो कर आगे बढ़ता है तथा अन्ततः निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुँच जाता है।
हे मोक्षप्रिय ! निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्राप्त परमानन्द का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। आपको स्वयं समाधि की स्थिति में इसका अनुभव करना होगा। निर्विकल्प समाधि का आनन्दमय अनुभव सविकल्प समाधि के अनुभव से अधिक श्रेष्ठ है।
१४. निद्रा तथा समाधि
मोक्षप्रिय ने कहा—हे पुरुषोत्तम! मैं समाधि के स्वरूप तथा उसके सारतत्त्व को समझ गया हूँ। अब कृपा करके निद्रा तथा समाधि का अन्तर स्पष्ट करें।
गुरुदेव ने उत्तर दिया— हे मोक्षप्रिय ! यह बहुत सुन्दर प्रश्न है।
निद्रा जड़ता की अवस्था है। समाधि शुद्ध चेतना की अवस्था है। जब व्यक्ति सो कर उठता है, तब उसे अपनी आत्मा के इन्द्रियातीत ज्ञान का कोई अनुभव नहीं होता। वह उस समय बिलकुल उदास तथा स्फूर्तिहीन होता है। परन्तु जब वह समाधि-अवस्था से जाग्रत अवस्था में आता है, तब वह आत्मज्ञान सम्पन्न होता है। वह आपके समस्त भ्रमों को दूर कर सकता है। वह आपको प्रेरणा प्रदान करके आपका उन्नयन कर सकता है। वह स्वयं ब्रह्म ही होता है।
समाधि निद्रा-रहित निद्रा है। समाधि में योगी को बाह्य संसार की चेतना नहीं रहती। उस समय वह परमानन्द और प्रज्ञा के सागर में निमज्जित रहता है।
हे मोक्षप्रिय ! निद्रावस्था गहन तम की अवस्था होती है। उस समय जीवात्मा कारण- शरीर में स्थित रहती है; परन्तु समाधि-अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म में या सच्चिदानन्दस्वरूप में स्थित रहती है।
जाग्रतावस्था में गहन निद्रा की अवस्था का लोप हो जाता है। परिवर्तित होती हुई अवस्था अवास्तविक होती है। समाधि (या परम चेतना) की अवस्था में योगी को साक्षी रूप में तीनों अवस्थाओं की चेतना रहती है। यह चेतना सदैव बनी रहती है। यही वास्तविक अवस्था है।
निद्रावस्था में वासना तथा संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म रूप में रहते हैं; परन्तु समाधि में वे सम्पूर्णतः ज्ञानाग्नि में जल कर भस्म हो जाते हैं।
हे मोक्षप्रिय ! अपने अहं, वासनाओं तथा पंचेन्द्रियों को इस अग्नि में डाल कर नष्ट कर दें तथा इस निद्रा रहित निद्रा (समाधि) के परमानन्द का अनुभव करें।
१५. समाधि
मोक्षप्रिय ने कहा-भाग्यशाली स्वामी जी! मुझे योग के पूर्ववर्ती अंगों का स्पष्ट ज्ञान हो गया है। अब कृपया समाधि के बारे में बतायें।
गुरुदेव ने उत्तर दिया हे मोक्षप्रिय ! इसकी विवेचन करना बहुत कठिन है। शब्द स्पष्ट और भाषा इस उच्च उन्नत स्थिति का भली प्रकार वर्णन करने में असमर्थ है।
समाधि परम चेतना की स्थिति है। यह ब्रह्म से सम्मिलन की स्थिति है। समाधि की अवस्था में मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ कार्य करना बन्द कर देती हैं। ये तीनों मूल प्रकृति में विलीन हो जाती हैं।
समाधि परमानन्द तथा शाश्वत प्रज्ञा की अवस्था है। इस अवस्था में सभी द्विविधताएँ समग्र रूप से नष्ट हो जाती हैं।
इस अवस्था का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अपने प्रत्यक्ष अन्तज्ञान से आपको इस अवस्था का अनुभव करना होगा। क्या आप मिसरी के स्वाद या दाम्पतिक सुख का वर्णन कर सकते हैं।
समाधि ब्रह्म की व्यक्तिपरक चेतना है। सभी दृश्य तथा पदार्थ उस परम अदृश्य में विलीन हो जाते हैं। जीवात्मा वही बन जाती है, जिसके बारे में वह सोचा करती है।
प्रारम्भ में राजयोगी तथा भक्त का अनुभव द्विविध होता है। बाद में वे भी परब्रह्म के अद्वैत परमानन्द का अनुभव करने लगते हैं। समाधि दो प्रकार की होती है—सविकल्प तथा निर्विकल्प । सविकल्प-समाधि में मात्र एक विचार होता है एवं ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय के त्रिक की सत्ता समाप्त हो जाती है। एक भी विचार शेष नहीं रहता।
हे मोक्षप्रिय! कुछ अज्ञानी साधक गहन निद्रा तथा तमस् को समाधि समझते हैं। वे आंखें बन्द कर लेते हैं और समझने लगते हैं कि वे समाधिस्थ हो गये। समाधि पूर्ण आत्म जागरूकता की स्थिति है। समाधि की अवस्था में प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है।
मन की चंचलता, निद्रा, कामनाएं, असावधानी, अनिश्चय, सूक्ष्म वासनाएं, रोग, सविकल्प समाधि का आनन्द सन्देह, आध्यात्मिक दर्प, सांस्थानिक अभिमान व निर्विकल्प समाधि की बाधाएं हैं।
हे मोक्षप्रिय! कठिन परिश्रम करें। गुरु तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। एकान्त में रहें। अनवरत रूप से ध्यान करें। आपको समाधि का परमानन्द प्राप्त होगा ।
१६. योगसार उपनिषद् के अनुसार ध्यानयोग
"यं कंचिद्विषये बाह्यमाभ्यन्तरं वा अनुसन्दधोत्यस्य चित्तैकाग्रह्यं धारणा- किसी बाह्य या आन्तरिक विचार, बिन्दु या पदार्थ पर मन को केन्द्रित करना धारण या एकाग्रता है" (मन्त्र : ११) ।
यह कहना बहुत कठिन है कि एकाग्रता कहाँ समाप्त होती है और ध्यान कहाँ प्रारम्भ होता है। एकाग्रता के बाद ध्यान की स्थिति आती है।
मन की स्थिरता को एकाग्रता कहते हैं। यदि आप दुचित्तापन के समस्त कारणों को दूर कर सकें, तो एकाग्रता की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। एक सच्चा ब्रह्मचारी (जिसने अपने वीर्य की रक्षा की है) मन को भली प्रकार एकाग्र कर सकता है। एकाग्रता के पदार्थ की अनुपस्थिति में भी उसका स्पष्ट मानस-दर्शन करने की क्षमता आपमें होनी चाहिए। क्षण-भर में ही आपके सामने उसका मानसिक चित्र उभर कर आ जाना चाहिए। यदि आपने एकाग्रता का अभ्यास भली प्रकार किया है, तो आपके लिए यह बिलकुल कठिन नहीं होगा। जिसने अपनी इन्द्रियों को विभिन्न पदार्थों से हटा कर प्रत्याहार में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भली प्रकार एकाग्रता का अभ्यास कर सकता है। आपको अध्यात्म मार्ग पर धीरे-धीरे प्रत्येक अवस्था से होते हुए बढ़ना होगा। यम, नियम, आसन तथा प्रत्याहार की आधारशिला निर्मित करके ही धारणा, ध्यान और समाधि का भवन सफलतापूर्वक निर्मित किया जा सकता है।
आसन बहिरंग साधना है। ध्यान अन्तरंग साधना है। ध्यान और समाधि की तुलना में धारणा भी बहिरंग साधना हो जाती है। जो स्थिरतापूर्वक आसन में रह सकता है और जिसने प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी योग- नाड़ियों तथा प्राणमय कोश को शुद्ध कर लिया है, वह सरलता से अपने मन को एकाग्र कर सकता है। आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा तथा सहस्रार चक्रों में से किसी पर या नासिकाग्र-बिन्दु या जिह्वा के अग्र भाग पर आन्तरिक रूप से या किसी देवी-देवता के चित्र - हरि, हर, कृष्ण या देवी पर बाह्यतः एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। आप घड़ी की टिक-टिक की आवाज़ या मोमबत्ती की लौ, दीवाल पर बने हुए किसी काले बिन्दु, पेंसिल, गुलाब के फूल या किसी भी सुखद पदार्थ पर मन को एकाग्र कर सकते हैं। यह स्थूल एकाग्रता है। जब तक मन को टिकाने के लिए कोई पदार्थ नहीं होगा, तब तक मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। मन को किसी भी सुखद पदार्थ (जैसे चमेली का फूल, आम, सन्तरा प्रिय मित्र) पर सरलतापूर्वक टिकाया जा सकता है प्रारम्भ में मन को किसी ऐसे पदार्थ पर टिकाना कठिन है जिसे यह पसन्द नहीं करता यथा— विष्ठा, नाग, शत्रु, कुरूप चेहरा। जब तक मन एकाग्रता के पदार्थ पर भली प्रकार न टिकने लगे, तक एकाग्रता का अभ्यास करते रहे। जब मन एकाग्रता के पदार्थ से हटने लगे, तब बार-बार उस पदार्थ पर वापस ले आयें। गीता (६-२६) में भगवान् कृष्ण कहते हैं:
यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ।।
"यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरत है, उस-उस से रोक कर बारम्बार परमात्मा में ही निरोध करें।"
यदि आप अपनी एकाग्रता की शक्ति का विकास करना चाहते हैं, तो आपको अपने सांसारिक कार्य-कलापों में कमी लानी होगी। इसी को व्यवहार-क्षय कहते हैं आपको प्रतिदिन दो घण्टे तक मौन-व्रत का पालन करना होगा। जिस व्यक्ति का मनोविकारों से तथा बेतुकी कामनाओं के चिन्तन से भरा होता है, वह एक क्षण के लिए भी किसी पदार्थ पर अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता। उसका मन गुब्बारे की तरह इधर-उधर डोलता रहता है। अपने श्वासों का नियमन करें और उन पर नियन्त्रण प्राप्त करें। अपनी इन्द्रियों को अपने अधीन कर लें और तब मन को किसी सुखकर पदार्थ पर केन्द्रित करें। उस पदार्थ के साथ पवित्रता और शुचिता के विचारों को सम्बद्ध करें।
आप भ्रूमध्य-बिन्दु (त्रिकुटी) पर भी मन को एकाग्र कर सकते हैं। आप दाहिने कान से सुनायी पड़ने वाली अनाहत ध्वनि पर भी मन को एकाग्र कर सकते है। आप के चित्र पर भी एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। हाथ में बाँसुरी लिये हुए भगवान् कृष्ण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए भगवान् विष्णु का चित्र भी एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त है। आप अपने गुरु या किसी सन्त-महात्मा के चित्र पर भी मन को एकाग्र कर सकते हैं। वेदान्ती साधक आत्मा पर मन को एकाग्र कर सकते हैं। यही उनकी धारणा है।
धारणा अष्टांगयोग (अथवा महर्षि पतंजलि के राजयोग) की छठी अवस्था है। धारणा में मन की केवल एक वृत्ति रहती है, मन में केवल एक ही पदार्थ का चित्र उभरता है तथा मन के अन्य कार्य-कलाप रुक जाते हैं। जो आधा या एक घण्टे के लिए सफलतापूर्वक एकाग्रता का अभ्यास कर लेता है, उसे अतीन्द्रिय क्षमताएँ प्राप्त होती हैं। वह स्वयं बहुत शक्तिशाली बन जाता है।
जब हठयोगी षट्चक्रों पर एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, तब वे उन चक्रों के अधिष्ठातृ-देवताओं (गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव) पर मन को केन्द्रित करते हैं। प्राणायाम से अपनी श्वासों को नियन्त्रित करें। प्रत्याहार से अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखें और तब मन को सगुण या निर्गुण ब्रह्म पर केन्द्रित करें। हठयोग के अनुसार जो योगी २० मिनट तक कुम्भक के द्वारा अपनी श्वास रोक सकता है, वह धारणा का अभ्यास सफलतापूर्वक कर सकता है। उसका मन बिलकुल शान्त हो जाता है। प्राणायाम से मन स्थिर रहता है, विक्षेप समाप्त हो जाता है तथा एकाग्रता की क्षमता में विकास होता है। जो जिह्वा फ्रीनम् (frenum lingua) को काट कर तथा जीभ को लम्बी करके और उसे ऊपर ले जाते हुए तालू के छिद्र में लगा कर खेचरी का अभ्यास करते हैं, वे एकाग्रता (धारणा) का अभ्यास सफलतापूर्वक कर लेते हैं।
जो एकाग्रता का अभ्यास कर लेते हैं, उनका क्रम विकास तेजी से होता है। वे किसी भी कार्य को वैज्ञानिक परिशुद्धता और निपुणता से कर सकते हैं। जो काम साधारणतः छह घण्टों में पूरा किया जाता है, उसे एकाग्रता का सफल अभ्यासी आधे घण्टे में पूरा कर लेता है। यही बात किसी पुस्तक के अध्ययन पर भी लागू होती है। एकाग्रता से उमड़ती हुई भावनाएँ शुद्ध तथा शान्त होती हैं, विचार तरंगों को शक्ति मिलती है तथा विचार स्पष्ट बनते हैं। एकाग्रता से भौतिक विकास में भी सहायता मिलती है। साधक चाहे व्यापारी हो या कर्मचारी, वह अपना कार्य पहले की अपेक्षा अधिक करने लगता है। जो-जो बातें पहले अस्पष्ट, अनिश्चित, कठिन, जटिल, सम्भ्रम उत्पन्न करने वाली तथा भ्रान्तिपूर्ण प्रतीत होती थीं, वे स्पष्ट निश्चित, सरल और बुद्धिगम्य बन जाती हैं। आप एकाग्रता से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो साधक नियमित रूप से एकाग्रता का अभ्यास करता है, उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। भूख में और तीव्र रोगों से ग्रसित होने की दशा में एकाग्रता का अभ्यास करना बहुत कठिन है। जो एकाग्रता का अभ्यास करता है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है तथा उसकी मानसिक दृष्टि बहुत स्पष्ट रहती है।
किसी शान्त कमरे में जायें। पद्मासन लगा कर बैठें। आँखें बन्द कर लें। किसी सेब का चिन्तन करने से क्या होता है, इस पर विचार करें। आप इसके रंग, रूप, आकार और इसके विभिन्न भागों (छिलकों, गूदा, बीज आदि) के बारे में सोच सकते हैं। आप उन स्थानों के बारे में सोच सकते हैं जहाँ से सेबों का आयात किया जाता है जैसे आस्ट्रेलिया या कश्मीर। आप सेब के खट्टे-मीठे स्वाद और पाचन तन्त्र तथा रक्त पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में सोच सकते हैं। साहचर्य के सिद्धान्त के अनुरूप अन्य सम्बन्धित फलों के विचार भी मन में आ सकते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य बाह्य विचार भी मन में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद मन भटकने भी लग सकता है। वह चार बजे स्टेशन पर किसी मित्र से मिलने की बात सोच सकता है। वह तौलिया या चाय-बिस्कुट खरीदने की बात भी सोच सकता है। वह पिछले दिन की किसी अप्रिय घटना को भी सोचने लग सकता है। किसी निश्चित विचार की धारा आपके मन में होनी चाहिए। इस विचार लगातार सोचे विचारणीय बात से असम्बद्ध किसी अन्य विचार को मन में प्रवेश न करते दें। इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस बात का भरसक प्रयत्न करेगा कि वह पुराने घिसे-पिटे रास्तों पर भागे। यह श्रमसाध्य प्रयत्न होगा। एकाग्रता में थोड़ी भी सफलता मिल जाने पर आपको अ लगने लगेगा। जिस प्रकार भौतिक स्तर पर गुरुत्वाकर्षण, संलाग (cohesion) आदि के नियम क्रियाशील होते हैं, उसी प्रकार मानसिक धरातल (या वैचारिक संसार) पर ि के कुछ निश्चित नियम—यथा साहचर्य, सापेक्षता, संसक्ति (contiguity) के नियम क्रियाशील होते हैं। एकाग्रता के अभ्यासी साधकों को ये नियम भली प्रकार समझते चाहिए। जब मन किसी पदार्थ के बारे में सोचता है, तब यह उसके गुणों और भागों के बारे में भी सोच सकता है। जब यह कारण के बारे में सोचता है, तब यह सम्बन्धित के बारे में भी सोच सकता है।
यदि आप एकाग्रतापूर्वक भगवद्गीता, रामायण या भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध को पढ़ें, तो हर बार आपको अपने स्वाध्याय के फलस्वरूप नये-नये विचार सूझेंगे। एकाग्रत से आपकी दृष्टि गहराई तक पहुँचती है। मानसिक चेतना के क्षेत्र में मानसिक पटल पर अनेकानेक सूक्ष्म और गूढ़ विचार कौंधते हैं। उनके गहन दार्शनिक पक्ष भी बोधगम्य होने लगते है। जब आप किसी पदार्थ पर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें, तो मन पर जोर न डालें। मन को इधर-उधर न भटकने दें।
एकाग्रता का अभ्यास करते समय यदि भावनाएं आपको विक्षुब्ध करें, तो चिन्ता न करें। भावनाओं का वेग स्वतः शान्त हो जायेगा। यदि आप उन भावनाओं को अपने ने दूर करना चाहेंगे, तो आपको अपनी इच्छा-शक्ति पर जोर डालना होगा। तटस्थ रहें। इस परिस्थितियों में वेदान्ती साधक कहते हैं- "मुझे तुम्हारी चिन्ता नहीं। दूर हो जाओ। मैं मानसिक वृत्तियों का साक्षी हूँ । भक्त साधक केवल प्रार्थना करते हैं और भगवान उनकी सहायता करते हैं।
एकाग्रता का अभ्यास करते समय मन को स्थूल सूक्ष्म, छोटी-बड़ी— सभी प्रकार की वस्तुओं पर केन्द्रित होने के लिए प्रशिक्षित करें। अन्ततः एकाग्रता का अच्छा अभ्यास होने लगेगा। तब जैसे ही आप एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए बैठेंगे, तदनुकूल मनःस्थिति सरलतापूर्वक तत्काल बन जायेगी। जब भी आप पुस्तक पढ़ें, उसे एकतापूर्वक पढ़ें। जल्दी-जल्दी पृष्ठ को उलटने से कोई लाभ नहीं होता। गीता का एक पृष्ठ पढ़ें, फिर उसे बन्द कर दें। जो कुछ पढ़ा है, उस पर मन को एकाग्र करें। महाभारत, भागवत तथा उपनिषदों में जहाँ-जहाँ आपने इस पृष्ठ के मूल भावों से मिलते-जुलते तथा उनके विरोधी भावों को पढ़ा हो, उन पर विचार करें।
नये अभ्यासी के लिए प्रारम्भ में एकाग्रता का अभ्यास क्लान्तिकर तथा नीरस होता है। उसको अपने मन-मस्तिष्क में नयी-नयी लीकें निर्मित करनी होती हैं। अभ्यास का कुछ समय व्यतीत होने के बाद उसको अपना मन एकाग्र करते समय बहुत अच्छा लगने लगता है। उसे एक नये प्रकार के आनन्द का अनुभव होने लगता है। यदि उसको एक दिन भी यह अनुभव न मिले, तो उसे व्याकुलता होने लगती है। सांसारिक विपत्तियों तथा क्लेशों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय एकाग्रता है। एकाग्रता का अभ्यास करना आपका एकमात्र कर्तव्य है । आपने एकाग्रता का अभ्यास करके आत्म-साक्षात्कार करने के लिए मानव-जन्म लिया है। एकाग्रता की तुलना में दानशीलता, राजसूय यज्ञ आदि कुछ भी नहीं हैं। वे इसके सामने मात्र खिलौने हैं।
वैराग्य, प्रत्याहार तथा एकाग्रता का अभ्यास करने से छितरी हुई चित्तवृत्तियाँ धीरे-धीरे सिमट कर एकत्र होने लगती हैं। स्थिरतापूर्वक अभ्यास करने से मन एक ही विचार-बिन्दु पर केन्द्रित होने लगता है कितना प्रसन्न और सशक्त होता है वह योगी, जिसका मन इस प्रकार का होता है ! वह पलक मारते ही ढेरों काम पूरे कर डालता है।
जो कभी-कभी एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, उनका मन भी कभी-कभी ही स्थिर हो पाता है। कभी-कभी मन भटकने लगता है और वह किसी भी प्रकार के उपयोग में आने के लिए बिलकुल अनुपयुक्त हो जाता है। आपका मन ऐसा होना चाहिए कि वह यथाशक्ति सर्वोत्तम ढंग से आपकी सभी आज्ञाओं का हर समय पालन कर सके। राजयोग का नियमित तथा व्यवस्थित अभ्यास करने से मन आज्ञाकारी तथा निशावान् बन जाता है।
योग भूमिकाएँ पाँच प्रकार की होती हैं—क्षिप्त, मूढ़ (विस्मरणशीलता), विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरूढ़ (भली प्रकार नियन्त्रित)। प्रतिदिन एकाग्रता का क्रमिक, व्यवस्थित तथा नियमित अभ्यास करने से भटकते हुए मन की वृत्तियाँ सिमट कर एकत्रित हो जाती हैं। मन एकाग्र होने लगता है। अन्ततः इसे उचित नियन्त्रण में तथा भली प्रकार से वश में रखा जा सकता है।
यदि साधक का लक्ष्य उचित या उपयुक्त नहीं है, तो उसका विकास धीमा होगा तथा उसमें बाधाएँ आयेंगी। जो अपने गत जन्मों के आध्यात्मिक संस्कार ले कर आता है, उसको एकाग्रता के अभ्यास में सफलता आसानी से मिलती है। जिस साधक की पृष्ठभूमि इन संस्कारों से विहीन होती है, उसकी सफलता के मार्ग में बाधाएँ आती हैं। जिसका स्वभाव वास्तव में अशुद्ध होता है तथा जिसकी बुद्धि कमजोर होती है, उसका विकास निर्बाध नहीं होता, उसका प्रातिभज्ञान भी मन्द रहता है; परन्तु जिसकी बुद्धि प्रखर होती है, उसका क्रम विकास तेजी से होता है तथा उसका प्रातिभज्ञान क्षिप्र हो जाता है जो साधक अज्ञान द्वारा विजित है, उसका प्रातिभज्ञान मन्द होता है। जिसने अज्ञान जीत लिया है, उसका प्रातिभज्ञान आशु हो जाता है।
"तैलधारावदनुसन्धाननैरन्तर्य ध्यानम् — किसी विचार के तैलधारावत् प्रवा की निरन्तरता ध्यान है" ( मन्त्र : १२ ) ।
ध्यान दो प्रकार का होता है— मूर्त (स्थूल) और अमूर्त। यदि आप स्थूल पदार्थ किसी चित्र पर मन को केन्द्रित करें, तो यह मूर्त ध्यान है। यदि आप किसी अमूर्त विचार या किसी गुण (दया, सहिष्णुता आदि) पर मन को केन्द्रित करें, तो यह अमूर्त ध्यान है प्रारम्भ में अभ्यासी को मूर्त ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मूर्त ध्यान की अपेक्षा अमूर्त ध्यान अधिक सरल होता है।
प्रत्याहार और धारणा (एकाग्रता) का भली प्रकार अभ्यास हो जाने के बाद साध को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यदि इन्द्रियाँ अभी भी उपद्रव मचाती है, मन किसी एक बिन्दु पर नहीं टिक पाता है, तो सौ सालों में भी ध्यान का अभ्यास नहीं हो पायेगा प्रत्येक अवस्था से गुजरते हुए क्रम से ही आगे बढ़ना चाहिए। जब मन इधर-उधर भाग लगे, तब उसे पूर्व-निश्चित विचार-बिन्दु पर वापस ले आना चाहिए। साधक को अपनी आवश्यकताएँ कम करके उच्छृंखल तथा निरर्थक कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए केवल कामना-रहित व्यक्ति ही शान्त बैठ कर ध्यान का अभ्यास कर सकता है। सात्त्वि हलका भोजन तथा ब्रह्मचर्य — ये ध्यानाभ्यास की पूर्वापेक्षाएँ हैं ।
चेतना दो प्रकार की होती है— संकेन्द्रित चेतना तथा औपान्तिक चेतना । जब आप त्रिकुटी (भ्रूमध्य-बिन्दु) पर मन को केन्द्रित करते हैं, तब आपकी संकेन्द्रित चेतना त्रिकुट पर होती है। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं और कोई मक्खी आपके बायें हाथ पर बै जाती है और आप उसे दाहिने हाथ से भगा देते हैं, तब मक्खी के प्रति आपकी चेतन औपान्तिक चेतना कहलाती है।
जो बीज एक क्षण के लिए भी आग में डाल दिया जाता है, वह निश्चित ही उर्वर भूमि में भी अंकुरित नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऐसे मन से जो थोड़ी देर के लिए घ्यान का अभ्यास करता है, परन्तु ऐन्द्रिय पदार्थों की तरफ भी दौड़ता है, योगाभ्यास सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।
"समाधिर्द्विविधः सम्प्रज्ञातोऽसम्प्रज्ञातश्चेति—समाधि दो प्रकार की होती है— सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात" (मन्त्र : १३) ।
समाधि परम चेतना की एक अवस्था है, जिसमें योगी को परा-ऐन्द्रिय अनुभव होते हैं। समाधि दो प्रकार की होती है-सम्प्रज्ञात (सबीज या सविकल्प) तथा असम्प्रज्ञात (निर्बीज या निर्विकल्प ) । सविकल्प समाधि में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय (की त्रिपुटी) की सत्ता रहती है। मन को टिकने के लिए एक आधार रहता है। संस्कार दग्ध नहीं होते । निर्विकल्प समाधि में न त्रिपुटी होती है और न आलम्बन होता है। समस्त संस्कार परिदग्ध हो जाते हैं। केवल निर्विकल्प समाधि ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करके परम ज्ञान और परमानन्द प्रदान कर सकती है। निर्विकल्प समाधि भी कई प्रकार की होती है— सवितर्क और निर्वितर्क, सविचार तथा निर्विचार, सानन्द और अस्मिता ।
जब आप असम्प्रज्ञात-समाधि (निर्विकल्प स्थिति) में प्रवेश करके राजयोग में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तब समस्त संस्कार तथा वासनाएँ—जिनके कारण बार-बार जन्म लेना पड़ता है— पूर्णतः भस्मीभूत हो जाते हैं। मन रूपी भँवर में उत्पन्न होने वाली समस्त वृत्तियों की तरंगें भी नियन्त्रित हो जाती हैं। पंचक्लेश-अविद्या, अस्मिता (अहंकार), राग, द्वेष तथा अभिनिवेश (जीवन के प्रति आसक्ति) नष्ट हो जाते हैं। कर्म-बन्धन भी विनष्ट हो जाते हैं। मन और इन्द्रियों को नियन्त्रित करें, कामना-रहित हो जायें, सहिष्णु बनें, चिन्तन-मनन करें। आत्मा में आत्मा का दर्शन करें। समाधि परम कल्याण (निश्रेयस) तथा अभ्युदय (उत्कर्ष) प्रदान करती है। यह मोक्ष (जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति) भी प्रदान करती है। अस्मिता आदि क्लेशों का मूल अविद्या ही है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर अविद्या नष्ट जाती है। मूल कारण (अविद्या) के नष्ट हो जाने से अहंकार आदि भी नष्ट हो जाते हैं।
असम्प्रज्ञात-समाधि की अवस्था में मन की समस्त वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं। सभी अवशिष्ट संस्कार भी विदग्ध हो जाते हैं। यह राजयोग की सर्वोच्च स्थिति है। इसे निर्बीज तथा निर्विकल्प समाधि कहते हैं।
राजयोग में धर्ममेघ का अर्थ होता है पुण्य का बादल । जिस प्रकार बादल वर्षा करते हैं, उसी प्रकार धर्ममेघ-समाधि भी योगियों पर सर्वज्ञता के गुण तथा सिद्धियों की वर्षा करती है। जीवन की अवस्था तथा जीवन के अनुभवों का बीज कर्म ही है। निर्बीज-समाधि कर्म के बीजों को परिदग्ध कर देती है।
ज्ञानी सन्त की दृष्टि
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी सब प्राणियों को ब्रह्म में तथा ब्रह्म को सभी प्राण में देखता है। उसकी दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। वह संसार निर्भीक हो कर विचरण करता है।
निज स्वरूप में स्थित आत्मसाक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति का यही अनुभव होता है एक आत्मज्ञानी की यही दृष्टि होती है। उसके जीवन में परस्पर दूरी उत्पन्न करने वाली अभेद्य सीमा रेखाएं समाप्त हो जाती हैं।
वह न पक्षपात करता है और न किसी वस्तु या व्यक्ति से घृणा । वह वर्णो तथा आश्रमों की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। वह किसी भी व्यक्ति से भोजन प्राप्त कर लेता है और कहीं भी सो जाता है। समाज में मनुष्यों द्वारा बनाये गये नियमों से वह बंधा हुआ नहीं होता। जन-मत का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका यह अर्थ नहीं कि वह किसी आचार संहिता का पालन नहीं करता। वह जो कुछ भी करता है, पूर्णतः शास्त्रानुकूल होता है। यदि सोते-सोते बोल पड़ने वाले किसी व्यक्ति से पूछें "क्या तुम कल रात कुछ बोल रहे थे ?" वह कहेगा- "नहीं, मैं तो नहीं बोला इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है।” सांसारिक कार्य-कलापों में रत ज्ञानी का अनुभव इसी प्रकार का होता है। उसके लिए सांसारिक कर्म बच्चे के की होते हैं, उसकी ब्रह्म-चेतना उस चोर नारी की तरह (द्विविध प्रकार की) होती है। जो घर का काम-काज करती रहती है, परन्तु जिसका मन अपने प्रेमी के पास ही रहता है अथवा उस कौवे की तरह होती है, जो अपनी एक ही पुतली को दोनों नेत्र गोलकों में घुमा कस इधर-उधर देखता है। वह समस्त संसार को अपने अन्दर देखता है। उसके लिए कोई वस्तु उसके बाहर नहीं है। उसके अन्दर अज्ञान (लेशाविद्या) के शेष रह जाने के कारण वह विचरण करता है, खाता-पीता है और सोता है। यदि किसी पात्र में हींग या (कटा हुआ) प्याज रख दिया जाये और फिर उसे निकाल कर पात्र को साफ किया जाये, तो उसमें रखी हुई वस्तु की गन्ध बनी रहती है। इसी प्रकार ज्ञानी के भी अन्तःकरण में अज्ञा का कुछ-न-कुछ अंश अवश्य बचा रहता है। इसी कारण वह सांसारिक क्रिया-कल करता रहता है।
१७. वेदान्तसार उपनिषद् के अनुसार ध्यान में बाधाएँ
"लयविक्षेपकषायरसास्वादाश्चत्वारोऽन्तराया आत्मबोधस्य-लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद –—ये आत्म-साक्षात्कार के मार्ग की चार प्रमुख बाधाएँ हैं" ( मन्त्र : ७) ।
निद्रा ही लय है। गहन निद्रा के पुराने संस्कारों के कारण विषय-पदार्थों से उपरत होते ही मन सुषुप्ति में प्रवेश करता है। साधक को अपने मन को गहरी निद्रा की स्थिति में प्रवेश करने से रोक कर उसे आत्मा पर केन्द्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे सदैव सावधान रहना चाहिए। आपके भरसक प्रयत्न करने पर यदि नींद का प्रभाव समाप्त नहीं होता है, तब आपको नींद लाने वाले कारणों का पता लगा कर उन्हें दूर करना होगा। इसके बाद आपको ध्यान का अभ्यास दोबारा करना होगा। अपच, गरिष्ठ भोजन, अति-भ्रमण, रात्रि काल में अपर्याप्त शयन-इन कारणों से ध्यान करते समय नींद आती - है। यदि आप रात में ठीक से न सो पाये हों, तो कभी-कभी अगले दिन दोपहर के समय थोड़ा आराम कर सकते हैं; परन्तु दिन के समय नियमित रूप से सोने के आदी न बनें। जब तक बहुत अधिक भूख न लगे, तब तक भोजन न करें। इस प्रकार अपच को दूर किया जा सकता है। आवश्यकता से अधिक न सोयें। मिताहारी बनें। जब पेट का तीन-चौथाई भाग भर जाये तथा थोड़ा और खाने की इच्छा बनी रहे, तभी खाना बन्द कर देना चाहिए। पेट को इसके लिए अभ्यस्त बना लें। अति-भ्रमण न करें। प्राणायाम के अभ्यास से भी लय पर नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है।
जब मन को निद्रा से उपरत कर लिया जाता है, तब भी वह ध्यान की स्थिति में प्रवेश नहीं करता। वह जाग्रत अवस्था के संस्कारों के वश में हो कर बार-बार ऐन्द्रिय सुखों के बारे में सोचता है तथा इच्छित पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यही विक्षेप है। विवेक और विचार द्वारा आपको बार-बार मन को उसके द्वारा इच्छित पदार्थों से हटा लेना चाहिए। आपको बाध-दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि, दोष-दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए। यह संसार अवास्तविक है—यह मिथ्या दृष्टि है। इस संसार का - अस्तित्व कभी भी नहीं रहता—यह बाध दृष्टि है। मानवीय क्लेशों के मूल कारण ऐन्द्रिय सुख हैं—यह दोष -दृष्टि है। उपर्युक्त उपाय से विक्षेप को दूर करें और बार-बार ध्यान का अभ्यास करें। जिस प्रकार बाज के द्वारा पीछा किये जाने पर पक्षी किसी घर में प्रवेश करता है और वहाँ उपयुक्त आश्रय स्थल न पा कर शीघ्र ही वहाँ से बाहर निकल आता है, उसी प्रकार जब मन सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्मा को उपयुक्त आश्रय स्थल के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, तब वह ऐन्द्रिय पदार्थों में भटकने के लिए बाहर निकल आता है। मन की यह बहिर्मुखी प्रवृत्ति विक्षेप है।
लय और विक्षेप को दूर करके जब मन अन्तर्मुखी हो जाता है, तब भी यह ध्यान की स्थिति में प्रवेश नहीं करना चाहता। छिपी हुई बलवती वासनाओं राग के प्रभाव के वश में हो कर यह पदार्थों में आसक्त हो जाता है। तब यह दुःख जाता है। इस समय मन में किसी एक विचार-बिन्दु पर एकाग्र होने की क्षमता रहती है। यह समाधि की स्थिति नहीं है। यही कषाय है। यह मनोराज्य है। इस स्थिति में म किले बनाता रहता है; पत्नी, पुत्र, धन के बारे में सोचता रहता है। यह बाह्य राग है। मन हवाई भूत के बारे में चिन्तन करता है तथा भविष्य के लिए योजनाएँ बनाता है। यह आन्तर-राग है। विक्षेप को दूर करने के लिए आपने जो उपाय किये थे, उन्हीं उपायों से आप कषाय को भी दूर कर सकते हैं।
वाह्य विषायाकार-वृत्ति विक्षेप है। जो वृति अन्दर से राग के संस्कारों के प्रभाव से उत्पन्न होती है, उसे कषाय कहते है। साधक कषाय को समाधि समझने की भूल कर बैठते हैं। आपको सावधानीपूर्वक इन दोनों का भेद समझ लेना चाहिए।
विक्षेप के दूर होते ही सविकल्प समाधि का आनन्द प्रकट होने लगता है। वह - रसास्वाद है। निर्विकल्प समाधि का परमानन्द प्राप्त करने में यह रसास्वाद एक बाधा ही है । इस रसास्वाद का आनन्द उसी प्रकार का है, जैसा कि कुली को अपने शिर का बोझ उतारने के बाद अथवा किसी गुप्त खजाने पर पहरा देने वाले साँप को मार डालने पर मिलता है; परन्तु वास्तविक आनन्द तो तब ही प्राप्त होता है, जब वह खजाने को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जब साधक निर्विकल्प समाधि के परमानन्द का अनुभव करें लगता है, तब वह अपनी साधना के चरम बिन्दु पर पहुँच पाता है। साँप को मारना विक्षेप को दूर करने के समान है।
जब ध्यान का अभ्यास किया जाता है, तब कई प्रकार की बाधाएँ सामने आती हैं— जैसे असम्यक् विचार, अधीरता, आलस्य, भोग-वृत्ति, वैषयिक तथा अपवित्र विचार । सम्यक् विचार तथा विवेक के द्वारा इन बाधाओं को दूर करें।
राग और तम मन में घुस कर अधिकार जमाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। उन्हें विवेक, विचार और वैराग्य की सहायता से हटा दें। धैर्य के अभ्यास द्वारा अधीरता को दूर करें। बार-बार शम, दम तथा उपरति का अभ्यास करें। आत्मा-सम्बन्धी विचार अपवित्र विचारों को नष्ट कर देंगे। आसन, प्राणायाम तथा सुपाच्य सात्त्विक आहार आलस्य को समाप्त करेगा।
१८. ध्यानयोग का सार-संक्षेप
धारणा
धारणा क्या है?
एकाग्रता ही धारणा है। यह किसी बाह्य पदार्थ या आन्तरिक बिन्दु पर मन को केन्द्रित करना है।
एकाग्रता पूर्ण रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है। एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए मन को अन्तर्मुखी होना चाहिए।
यदि आप किसी बिन्दु पर अपने मन को १२ सेकण्ड तक केन्द्रित कर सकें, तो यह धारणा है। इतनी अवधि की १२ धारणाएँ १ ध्यान के बराबर हैं। इस प्रकार के १२ घ्यानों को समाधि कहते हैं।
धारणा के सहयोगी साधन
अवधान (attention) की क्षमता का विकास करें। आपकी एकाग्रता विकसित होगी।
एकाग्रता के लिए मन को शान्त रखें।
सदैव प्रफुल्लित रहें। तभी आप एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं।
एकाग्रता का अभ्यास नियमित रूप से करें। एक ही स्थान तथा नियत समय (४ बजे प्रातः) पर अभ्यास करें।
ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, आवश्यकताओं तथा कार्य-कलापों का न्यूनीकरण, विरक्ति, मौन, इन्द्रिय-निग्रह, जप, क्रोध पर नियन्त्रण, समाचार-पत्र, उपन्यास आदि न पढ़ना, सिनेमा न देखना ये धारणा के सहयोगी साधन हैं।
जप तथा कीर्तन से एकाग्रता में वृद्धि होती है।
एकाग्रता का अभ्यास करते समय किसी एक ही विचार - बिन्दु पर मन को केन्द्रित करें।
धैर्यपूर्वक तथा दीर्घ काल तक एकाग्रता का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है।
एक दिन के लिए भी अभ्यास करना न छोड़ें। एक बार अभ्यास छूट जाने पर पुरानी गति को पकड़ पाना कठिन हो जाता है।
एकाग्रता का अभ्यास कैसे करें
उमड़ती हुई भावनाओं तथा विचारों को शान्त करें। केवल तभी आप एक अभ्यास कर सकेंगे।
प्रारम्भ में किसी आकार- फूल, भगवान् बुद्ध की आकृति, स्वप्न का दृश्य, हृदय प्रदेश का देदीप्यमान प्रकाश, किसी सन्त महात्मा के चित्र या इष्टदेवता पर मन को एकाग्र करें।
भक्त साधक हृदय पर, राजयोगी भ्रूमध्य-स्थित त्रिकुटीपर तथा वेदान्ती साधक त्रिकुटी या शिर के शीर्ष भाग पर मन को एकाग्र करते हैं।
आप नासिकाग्र-बिन्दु या नाभि या मेरुदण्ड की अन्तिम कशेरुका के नीचे मूल पर भी मन को एकाग्र कर सकते हैं।
१. इष्टदेव पर-
ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जायें। अपने समक्ष इष्टदेव का चित्र रख लें। टकटकी लगा कर चित्र को देखें। कुछ सेकण्ड के बाद आँखें बन्द कर और अपने हृदय के मध्य भाग में या भ्रूमध्य में चित्र का मानस-दर्शन करें।
जब मानस-दर्शन करते समय चित्र लुप्त होने लगे, तब दोबारा आँखें खोल स्थिर दृष्टि से चित्र को कुछ सेकण्ड तक देखें। आँखें बन्द करके फिर चित्र मानस-दर्शन करें।
२. ईसाई साधकों के लिए-
प्रभु यीशु के भक्त उनके चित्र या क्रूस पर उपर्युक्त प्रकार से मन को एकाग्र कर सकते हैं।
३. स्थूल आकार -
दीवाल में बने काले बिन्दु, मोमबत्ती की लौ, चमकदार तारे, चन्द्रमा, ॐ के या किसी सुखकर पदार्थ पर एकाग्रता का अभ्यास करें।
जब आँखों पर जोर पड़ने लगे, तो उन्हें बन्द करके सम्बन्धित पदार्थों का मानस-दर्शन करें । मन इधर-उधर भागे, तो उसे एकाग्रता के पदार्थ पर वापस ले आयें ।
भावुक प्रकृति के अभ्यासियों के लिए चन्द्रमा पर मन एकाग्र करना लाभदायक होगा। मोमबत्ती की लौ पर एकाग्रता का अभ्यास करने से ऋषियों और देवताओं के दर्शन होते हैं।
४. सूक्ष्म विधियाँ-
प्रेम, करुणा, दया अथवा किसी भी अमूर्त विचार (यथा-ईश्वर की अनन्तता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापिता) पर मन को एकाग्र करें।
किसी पुस्तक के दो या तीन पृष्ठ पढ़ें पुस्तक बन्द कर दें। जो कुछ आपने पढ़ा है, उस पर अपना अवधान संकेन्द्रित करें। किसी भी विचार को मन में न आने दें। अब अपने मन को आदेश दें कि वह समान विचारों को एक साथ रखते हुए उनका वर्गीकरण करे। विचारों के छोटे-छोटे समूह बना लें, फिर उनकी परस्पर तुलना करें। इस प्रकार आप सम्बन्धित विषय का अमित ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। आपकी स्मृति तीव्र हो जायेगी।
विस्तृत नीले आकाश के नीचे लेट कर उस पर एकाग्रता का अभ्यास करें। आपका मन आकाश की भाँति विस्तृत होने लगेगा। आपको अपने उन्नयन का अनुभव होगा। नीला आकाश देख कर आपको आत्मा की असीमता की याद आयेगी।
५. ध्वनियों पर-
ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठें। नेत्रों को बन्द करें। तर्जनी उँगली या रुई से कर्ण-छिद्रों को बन्द कर लें। विभिन्न प्रकार के अनाहत नादों (यथा-बाँसुरी या वायलिन का संगीत, नक्कारों, तूफान, पण्टियों की आवाजें मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, शंख-ध्वनि) को सुनने का प्रयत्न करें। एक समय में एक ही प्रकार की ध्वनि को सुनें । अन्यान्य पदार्थों में लगी हुई मन की वृत्तियों का प्रत्याहरण करके उन्हें उस ध्वनि में विलीन कर दें, जिसे सुनने का आप प्रयत्न रह रहे हैं। इससे मन स्थिर होगा। मन को सुरीली ध्वनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अतः इस विधि से मन को नियन्त्रित करना सरल होगा।
घड़ी की टिक-टिक की ध्वनि पर मन को एकाग्र करें। एकान्त स्थान में किसी नदी के तट पर बैठें। प्रवाहित होते हुए जल की ध्वनि पर मन को एकाग्र करें। आपको ॐ का गर्जन सुनायी पड़ेगा। यह ध्वनि अत्यन्त भावोत्तेजक तथा प्रेरणाप्रद होती है।
६. सूफी विधि-
अपने सामने एक दर्पण रखें। अपने प्रतिबिम्ब के भूमध्यबिन्दु पर मन को एकाग्र करें ।
७. त्रिकुटी पर
त्रिकुटी पर एकता का अभ्यास करने से मन को सरलता से नियन्त्रित किया जा सकता है।
त्रिकुटी पर गहन एकाग्रता हो जाने के परिणामस्वरूप आनन्द तथा अध्यात्मिक उन्माद का अनुभव होता है। तब अपने शरीर तथा प्रतिवेश का भान नहीं रहता। समस्त प्राण ऊर्ध्वदिशा — शिर की ओर जाने लगते हैं।
किसी स्फटिक या शालिग्राम पर टकटकी लगा कर देखने से एकाग्रता गहन होने लगती है। नासा-छिद्रों में अपनी श्वास पर भी आप एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। स्वास लेते समय 'सो' की तथा श्वास छोड़ते समय 'हं' की सूक्ष्म ध्वनि निकलती है।
सामान्य संकेत
जब मन थका हुआ न हो, तब एकाग्रता का अभ्यास न करें।
एकाग्रता का अभ्यास करते समय मन के साथ लड़ाई न करें।
जब असंगत विचार मन में उठे, तब उन पर ध्यान न दें। वे अपने-आप चले जायेंगे। उन्हें जबदस्ती न भगायें, अन्यथा वे प्रतिरोध करके मन में टिकने का प्रयास करेंगे। असंगत विचार दोगुनी शक्ति से मन में दोबारा प्रवेश करेंगे। इससे आपकी इच्छा-शक्ति पर बहुत जोर पड़ेगा। दिव्य विचारों का चिन्तन करें। तब अशुभ विचार धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगे।
एकाग्रता का अभ्यास स्थिरतापूर्वक तथा धीरे-धीरे करें। यदि मस्तिष्क में ताप का अनुभव होने लगे, तो ब्राह्मी आँवला तेल का प्रयोग करें।
मक्खन तथा मिसरी का प्रयोग करें। इससे शरीर में उण्ढक उत्पन्न होती है।
जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता की क्षमता का विकास करना होगा। आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत एकाग्रता ही है। एकाग्रता ज्ञान-द्वार को खोलने की कुंजी है।
ध्यान
ध्यान क्या है?
ध्येय के ज्ञान का अनवरत प्रवाह ध्यान है।
एकाग्रता (धारणा) के बाद ध्यान की स्थिति आती है। एकाग्रता ध्यान में विलीन हो जाती है।
ध्यान योग-निसेनी का सातवाँ डण्डा है।
एकाग्रता (धारणा), ध्यान तथा समाधि आन्तरिक साधनाएँ हैं।
जब आप धारणा, ध्यान तथा समाधि का अभ्यास एक ही समय में साथ-साथ करते हैं, तब वह संयम कहलाता है।
ऐन्द्रिय पदार्थों के चिन्तन से मन को मुक्त करना ही ध्यान है। ध्यानावस्था में मन मात्र ईश्वर का ही चिन्तन करता है।
ध्यान के लाभ
यदि आप नित्य आधे घण्टे तक ध्यान करते हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से शान्तिपूर्वक आप जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं।
ध्यान से पीड़ा, क्लेश और दुःखों का नाश होता है।
ध्यान सर्वाधिक प्रभावशाली मानसिक और शामक टॉनिक है।
ध्यान करते समय साधक की दिव्य ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध हो जाता है। इसका मन, नाड़ियों, इन्द्रियों तथा शरीर पर अत्यन्त हितकर और शामक प्रभाव पड़ता है।
ध्यान एक ऐसी गुह्य निसेनी है, जिससे हो कर योग का विद्यार्थी पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाता है।
ध्यान जीवन के अनेकानेक रहस्यों को प्रकट करने वाली कुंजी है। ध्यान प्रातिभज्ञान तथा परमानन्द के क्षेत्रों का प्रवेश द्वार है।
ध्यान की अवस्था में मन शान्त, अविक्षुब्ध और स्थिर हो जाता है। उस समय मन में केवल एक ही विचार रहता है।
गहन ध्यान की स्थिति एक दिन, एक सप्ताह अथवा एक मास में उपलब्ध नहीं होती। इस स्थिति में पहुँचने के लिए आपको दीर्घ काल तक कठिन परिश्रम करना होगा। धैर्य रखें। अध्यवसायी बनें। सावधान रहें। परिश्रमी बनें
आत्म-साक्षात्कार के लिए तीव्र विरक्ति की भावना तथा प्रबल आकांक्षा रखें । धीरे-धीरे आप गहन ध्यान तथा समाधि की अवस्था में प्रवेश करेंगे।
ध्यान करने से समस्त सन्देह धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगे।
एक रहस्यमय आन्तरिक स्वर आपका मार्ग-निर्देशन करेगा।
योग-निसेनी के अगले डण्डे के लिए पग रखते समय आपको आगे का मार्ग अपने-आप दिखायी पड़ने लगेगा।
ध्यान कैसे करें
प्रातः ४ और ६ बजे के बीच नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करें। इस समय मन शान्त तथा स्फूर्त रहता है। वातावरण भी शान्त रहता है। यह समय ध्यान के लिए अनुकूल है।
आपका ध्यान कक्ष अलग होना चाहिए। यदि ऐसा सम्भव न हो, तो परदा डाल कर किसी कमरे का एक कोना ध्यानाभ्यास के लिए अलग कर ले। यदि ध्यानाभ्यास करते समय मन तनावग्रस्त हो जाये, तो कुछ दिनों के लिए ध्यान की प्रत्येक बैठक समय कम कर दें और हलका ध्यान करें।
साधना काल में अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करें। अतियों पर न जायें । सदैव मध्यम मार्ग को अपनायें।
सगुण ध्यान
प्रारम्भ में ध्यान करने के लिए मन को स्थूल पदार्थ की आवश्यकता होती है।
शुरू-शुरू में किसी स्थूल आकार (जैसे इष्टदेव की मूर्ति, प्रभु यीशु, भगवान् बुद्ध पर ध्यान करें। यह सगुण ध्यान है।
भगवान् पर ध्यान करते समय उनके गुणों - सर्वशक्तिमत्ता, पूर्णता, शुचिता, स्वतन्त्रता का चिन्तन करें।
भगवान् के आकार में उनके शिर से पैर तक या पैर से शिर तक अपनी चेतना को घुमायें।
प्रभु यीशु पर ध्यान
ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जायें। अपने सामने प्रभु यीशु का एक चित्र रखें। आंखें खोल कर चित्र पर मन को तब तक एकाग्र करें, जब तक आपकी आंखों पर आयास न पड़ने लगे। उनके लम्बे-लम्बे केशों, सुन्दर दाढ़ी, गोल नेत्रों, वक्ष पर रखे क्रूस, शरीर के अन्य अवयवों तथा प्रभा मण्डल आदि पर अपनी चेतना को घुमायें ।
उनके दिव्य गुणों-प्रेम, उदारता, दया, सहिष्णुता का चिन्तन करें। उनके रोचक जीवन के विभिन्न आयामों, उनके द्वारा दिखाये गये चमत्कारों तथा उनकी असाधारण शक्तियों के बारे में भी सोचें। अब अपनी आँखें बन्द कर लें और चित्र का मानस-दर्शन करने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को बार-बार दोहरायें।
भगवान् हरि पर ध्यान
ध्यान के किसी आसन में बैठें। अपने सामने भगवान् हरि का चित्र रख लें। चित्र पर मन को एकाग्र करें; लेकिन मन को तनाव ग्रस्त न होने दें। उनके चरणों, पील-कौशेय परिधानों, हीरे से जड़ी हुई स्वर्णिम मालाओं, वक्षस्थल की कौस्तुभ मणि, मुख, कर्णफूलों, मुकुट, ऊपरी दाहिने हाथ के चक्र, ऊपरी बायें हाथ के शंख, निचले दाहिने हाथ की गदा और निचले बायें हाथ के पद्म पर अपनी चेतना को घुमायें। अब आँखें बन्द करके उनके चित्र का मानस-दर्शन करें। इस प्रक्रिया को बार-बार दोहरायें। भगवान् बुद्ध के भक्त इसी विधि से उनके आकार का ध्यान उनके विशिष्ट गुणों का चिन्तन करते हुए कर सकते हैं।
ॐ पर ध्यान
अपने सामने ॐ का चित्र रखें। खुले नेत्रों से इस चित्र पर मन को एकाग्र करें। मन पर बहुत जोर न डालें। ॐ का चिन्तन करते समय शाश्वतत्व, असीमता, अमरता आदि के विचारों के बारे में सोचें। यह भी सोचें कि मधुमक्खियों की गुनगुनाहट, कोयल के मधुर गीत, संगीत के सातों स्वर—ये सब ॐ से निःसृत हुए हैं। ॐ वेदों का सार है। कल्पना करें कि ॐ धनुष है, मन बाण है तथा ब्रह्म (ईश्वर) लक्ष्य है। सावधानी से लक्ष्य-बेध करें। जिस प्रकार अन्त में तीर और लक्ष्य एक हो जाते हैं, उसी प्रकार आप और ब्रह्म एक हो जायेंगे। ध्यान करते समय आप ॐ का उच्चारण भी कर सकते हैं। ॐ का अनुदात्त स्वराघात सभी पापों को भस्मीभूत कर देता है तथा उदात्त स्वराघात सब प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करता है। जो साधक ॐ का उच्चारण तथा ध्यान करता है, वह संसार के सभी सद्ग्रन्थों का ध्यान करता है।
अमूर्त ध्यान
सूर्य का तेज, चन्द्रमा की प्रभा तथा तारकों की द्युति का ध्यान करें।
समुद्र के वैभव और असीमता का ध्यान करें। फिर उसकी तुलना से ब्रह्म से करें । समुद्र की लहरों, फेन और हिमशैलों की तुलना विभिन्न सांसारिक नाम-रूपों से करें । सोचें कि आप समुद्र है। शान्त हो जायें। समुद्र के समान अपना विस्तार करें, विस्तार करते जायें।
हिमालय का ध्यान करें। सोचें- गंगोत्तरी के हिममय क्षेत्रों से निकल कर ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी होती हुई प्रवाहित हो रही है और अन्त में गंगा सागर के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हिमालय, गंगा और समुद्र (बंगाल खाड़ी) — केवल ये तीन विचार ही आपके मन में रहें। पहले गंगोत्तरी के हिममय क्षेत्र अपनी चेतना को ले जायें। फिर गंगा के प्रवाह पर से होते हुए उसे समुद्र तक से चेतना को इसी प्रकार घुमायें।
आकारहीन वायु की ओर टकटकी लगा कर देखे। वायु पर मन को एकाग्र कर वायु के सर्वव्यापक स्वरूप का ध्यान करें। यह ध्यान आपको नाम रूप-रहित ब्रह्म-जो एकमात्र जीवन्त सत्य है—के साक्षात्कार की ओर ले जायेगा।
अपनी श्वास के प्रवाह के प्रति जागरूक बनें। आपको 'सोऽहम्' की सूक्ष्म ध्वनि सुनायी पड़ेगी श्वास अन्दर लेते समय 'सो' की तथा छोड़ते समय 'हं' की ध्वनि । 'सोऽहम्' का अर्थ है— मैं वही हूँ। आपकी श्वास आपको परमात्मा के साथ आपकी अभिन्नता का स्मरण करा रही है। प्रति मिनट १५ की दर से आप सहज प्रतिदिन २१,६०० बार ‘सोऽहम्' का जप कर रहे हैं। 'सोऽहम्' के साथ सत्, चित तथा आनन्द, पूर्ण शुचिता, शान्ति, पूर्णता तथा प्रेम के विचारों को सम्बद्ध करें। मंत्र का जप करते समय अपने शरीर को नकारें तथा परम आत्मा के साथ अपनी अभिन्नता क अनुभव करें ।
निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करें । सोचें कि समस्त नाम-रूपों के मूल में जीवन्त परम शक्ति है । यह शक्ति सच्चिदानन्द-स्वरूप है तथा असीमता, शाश्वतत्व और अमरता के लक्षणों से सम्पन्न है—यथासमय ये लक्षण विशुद्ध निर्गुण ध्यान में विलीन हो जायेंगे ।
ध्यान के अनुभव
ध्यान करते समय शरीर के ऊपर उठने का अनुभव इस बात का द्योतक है है अभ्यासी शरीर की चेतना से परे जा रहा है।
यदि आप एकाग्रता (धारणा) और ध्यान का अभ्यास करें, तो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ और सिद्धियाँ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी; परन्तु सांसारिक लाभों प्राप्त करने के लिए इन शक्तियों की सहायता न लें। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आप इनका दुरुपयोग करेंगे। आप पतन के गहरे गर्त में गिर जायेंगे।
योग के मार्ग में सिद्धियाँ बाधाएँ हैं। वे प्रलोभन हैं। वे आपको समाधि-अवस्था में प्रवेश करने या जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती हैं। उनसे दूर रहें तथा सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें।
चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं होती। जब आपको चमत्कार का मूल कारण समझ में आ जाता है, तब वह (चमत्कार) आपके लिए एक साधारण घटना बन जाता है।
ध्यान की अवस्था में आपको हर्षोन्माद, आनन्दातिरेक तथा रोमांच का अनुभव होता है।
ध्यान में जब आपको ज्योति की कौंध दिखायी पड़े, तब भयभीत न हो जायें। यह असीम आनन्द का एक नवीन अनुभव होगा।
जब आप शरीर की चेतना से ऊपर उठ जायें, तब अकारण ही परेशान न हो जायें। साधना करते जायें। ईश्वर आपकी रक्षा करेगा और आपका मार्ग-निर्देशन करेगा। निर्भीक बनें। पीछे की ओर न देखें। आगे की ओर बढ़ें।
ज्योति की कौंध सत्य की एक झलक है। यह ऋतम्भरा प्रज्ञा है। यह सम्पूर्ण अनुभव नहीं है। यह सर्वोच्च अनुभव भी नहीं है।
भूमा की स्थिति को प्राप्त करें। यही चरम तथा अन्तिम अवस्था है। यही परम लक्ष्य है। यहीं पर ध्यान की अवस्था समाप्त होती है।
आपको विभिन्न प्रकार की अनाहत ध्वनियाँ सुनायी पड़ेंगी, यथा-घड़ियाल, बाँसुरी, वीणा, मृदंग, ढोल, मेघ गर्जन आदि की ध्वनियाँ ।
आपको भ्रमध्य-बिन्दु पर चमकदार प्रकाश दृष्टिगोचर होगा। यह प्रकाश स्फुलिंग, सूर्य, चन्द्रमा या तारकों के प्रकाश की तरह होता है। आपको अभेद दृष्टि प्राप्त होगी।
कभी-कभी आपको रंगीन—हरे, नीले, लाल आदि-प्रकाश दिखायी पड़ेंगे। किसी विशेष समय में किसी विशेष तत्त्व के उपस्थित रहने के कारण रंगीन प्रकाश दिखायी पड़ता है। पृथ्वी-तत्त्व में पीला प्रकाश, जल-तत्त्व में सफेद प्रकाश, अग्नि-तत्त्व में लाल प्रकाश, वायु-तत्त्व में धूमिल या हरा प्रकाश तथा आकाश-तत्त्व में नीला प्रकाश होता है। इन प्रकाशों को कोई महत्त्व न दें और साधना पथ पर आगे बढ़ते जायें ।
ध्यान में कभी-कभी आपको ऋषियों, महात्माओं, अधिष्ठातृ-देवताओं नित्य-सिद्धों, सूक्ष्म सत्ताओं आदि के दर्शन होते हैं। प्राकृतिक दृश्य, पहाड़, नीला आकाश, सुन्दर बाग-बगीचे आदि दिखायी पड़ते हैं।
कभी-कभी ध्यान की अवस्था में आप हवा में तैर भी सकते हैं। तब आपका शरीर आपके स्थूल शरीर से पृथक् हो जायेगा तथा आप सूक्ष्म लोकों में विचरण करेंगे।
आप ब्रह्मलोक-ब्रह्म या हिरण्यगर्भ का लोक—की भी यात्रा कर सकते हैं।
जो साधक ध्यान की प्रथम अवस्था में प्रवेश कर लेते हैं, उनका शरीर हलका है जाता है, स्वर मधुर हो जाता है तथा रूप-रंग सुन्दर हो जाता है। उनके चिन्तन में स्पष्ट आ जाती है। उनके द्वारा विसर्जित मल-मूत्र के परिमाण में भी कमी आ जाती है।
समाधि
समाधि क्या है?
समाधि परम चेतना की अवस्था है। परब्रह्म के साथ एकता ही समाधि है।
समाधि की अवस्था वर्णनातीत है। भाषा या अन्य किसी माध्यम से इसका वर्णन करना असम्भव है।
प्रत्यक्ष प्रातिभज्ञान के द्वारा आपको समाधि की अवस्था का स्वयं अनुभव करना होगा। क्या आप मिसरी के स्वाद का वर्णन कर सकते हैं? हाँ, इतना कहा जा सकता है कि समाधि की अवस्था आनन्द, प्रसन्नता और शान्ति से परिपूर्ण है; परन्तु इसका अनुभव साधक को स्वयं करना होगा।
समाधि में ध्याता की वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है। वह परम आत्मा के साथ मिल कर एक हो जाता है। जिस प्रकार कपूर अग्नि से अभिन्न हो जाता है, उसी प्रकार ध्याता ध्येय से अभिन्न हो जाता है।
जिस प्रकार सरिता सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा उस परमात्मा में मिल जाती है जो परम चेतना का सागर है।
समाधि का परमानन्दमय दिव्य अनुभव तभी प्राप्त होता है, जब मन और अहंकार विलीन हो जाते हैं।
कुछ मूर्ख लोग समझते हैं कि समाधि जड़ता की अवस्था है। यह धारणा त्रुटिपूर्ण है।
समाधि अवस्था एकता का तथा परम सत्ता से एकाकार होने का भव्य अनुभव है। समाधि एक इन्द्रियातीत अनुभव है। इस अवस्था में द्रष्टा और दृश्य मिल कर एक हो जाते हैं।
समाधि की अवस्था में साधक को बाह्य या आन्तरिक पदार्थों का भान नहीं रहता; चिन्तन, श्रवण, आघ्राण या अवलोकन की क्रियाएँ भी नहीं होतीं।
समाधि की अवस्था में प्रवेश करने का अधिकार प्रत्येक मानव को है।
समाधि के सहायक साधन
श्रद्धा, मन को एकाग्र करने की क्षमता, धारणा-शक्ति, ब्रह्मचर्य तथा प्रज्ञा समाधि-अवस्था में प्रवेश करने में सहायक होते हैं।
केवल ईश्वर की कृपा आपको निर्विकल्प समाधि के लोकोत्तर अनुभव के क्षेत्र में ले जा सकती है।
जड़ तथा चैतन्य-समाधि
हठयोगी द्वारा भूमि के अन्दर लगायी जाने वाली समाधि जड़-समाधि है। जड़-समाधि मात्र गहन निद्रा है। इस अवस्था में न लोकोत्तर अनुभव होते हैं और न दिव्य प्रज्ञा प्राप्त हो पाती है। संस्कार का क्षय भी नहीं हो पाता। मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता ।
चैतन्य-समाधि की अवस्था में पूर्ण चेतना (जागरूकता) बनी रहती है। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद साधक पुनः जन्म नहीं लेता। उसे दिव्य प्रज्ञा तथा मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
सविकल्प- समाधि
समाधि दो प्रकार की होती है—सविकल्प तथा निर्विकल्प। सविकल्प- समाधि को सम्प्रज्ञात या सबीज-समाधि भी कहते हैं। सविकल्प-समाधि में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की त्रिपुटी की सत्ता रहती है। एकाग्रता की स्थिति में ही सम्प्रज्ञात (या सविकल्प) समाधि में प्रवेश किया जा सकता है।
इस स्थिति में मन का आंशिक निरोध (inhibition) हो पाता है।
संस्कारों का क्षय नहीं होता है; इसीलिए इस अवस्था को सबीज-समाधि कहते हैं।
जब योगी (रजसू और तमस्-रहित) सात्त्विक मन का ध्यान करता है, तब उसे अपरिमित आनन्द प्राप्त होता है; इसीलिए इसे सानन्द-समाधि कहते हैं।
योगी को 'अहं अस्मि' की अनुभूति होती है; अतः इसे अस्मिता-समाधि भी कहते हैं।
निर्विकल्प- समाधि
निर्विकल्प- समाधि पूर्ण चेतना की अवस्था है।
ज्ञान और ज्ञेय मिल कर एक हो जाते हैं।
निर्विकल्प- समाधि में योगी बिना आँखों के देखता है, बिना जिह्वा के स्वाद लेता है, बिना कानों के सुनता है, बिना नाक के सूंघता है तथा बिना त्वचा के स्पर्श करता है।
इसी बात को इस प्रकार भी कहा गया है :
"अन्धे ने हीरे में छेद कर दिया। उँगली-विहीन व्यक्ति ने उसमें डोरा डाला।। ग्रीवा-विहीन व्यक्ति ने उसे पहना और जिह्वा विहीन ने उसकी प्रशंसा की।"
निर्विकल्प-समाधि को असम्प्रज्ञात या निर्बीज-समाधि भी कहा जाता है।
इस अवस्था में समस्त मानसिक क्रियाएँ निरुद्ध हो जाती हैं; इसी कारण असम्प्रज्ञात-समाधि कहते हैं।
जब मन का पूर्णतः निरोध (नियन्त्रण) हो जाये, तभी इस अवस्था में प्रवेश करन सम्भव होता है।
इस अवस्था में संस्कार पूर्णतः विदग्ध हो जाते हैं; इसी कारण इसे निर्बीज-समाधि कहते हैं।
केवल निर्विकल्प-समाधि ही पुनर्जन्म से मुक्ति प्रदान कर सकती है।
परन्तु, सत्य की मात्र झलक ही जन्म-मरण से मुक्ति नहीं दिला सकती।
आपको निर्विकल्प-समाधि की स्थिति में पूर्णतः अवस्थित होना होगा। केवल तभी पुनर्जन्म का बीज समग्र रूप से विदग्ध हो पायेगा ।
जब योगी निर्विकल्प समाधि की सर्वोच्च अवस्था में प्रवेश कर लेता है, तब योगाग्नि से उसके अवशेष कर्म दग्ध हो जाते हैं। वह जीते-जी तुरन्त ही मोक्ष प्राप्त लेता है। वह अमरता, सर्वोच्च भावातीत प्रज्ञा तथा शाश्वत परमानन्द को भी प्राप्त करता है।
निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रवेश करने के लिए परा-वैराग्य ही एकमात्र साधना है।
परा-वैराग्य में योगी अपने को प्रकृति तथा उसके परिणामों से पूर्णतः असम्बद्ध कर कर लेता है।
मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ पूर्णतः कार्य करना बन्द कर देती हैं। न तो कोई ध्वनि सुनायी पड़ती है, न कोई रूप दिखायी पड़ता है और न स्पर्श की अनुभूति होती है।
समस्त प्रकार के क्लेश (यथा— अज्ञान, अहंकार, रुचि, अरुचि, अभिनिवेश) नष्ट हो जाते हैं।
गुण अपने-अपने विषयों का सुख भोग चुके होते हैं; अतः वे भी पूर्ण रूप से कार्य करना बन्द कर देते हैं। योगी परम स्वतन्त्रता या कैवल्य की अवस्था में प्रवेश करता है।
वह सर्वज्ञ बन जाता है ।
भूत तथा भविष्य वर्तमान में मिल जाते हैं। सब-कुछ वर्तमान ही बन जाता है। सब कुछ 'यहीं' घटित होने लगता है।
योगी दिक्काल के परे हो जाता है।
सभी प्रकार के दुःख समाप्त हो जाते हैं। सारी विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। कर्मों के बीज दग्ध हो जाते हैं। समस्त भ्रमों का निवारण हो जाता है। शाश्वत स्वतन्त्रता का राज्य हो जाता है।
यह स्थिति तरंग-रहित सागर के समान होती है।
द्वितीय अध्याय
आनन्दामृत
१. अष्टांगयोग
सर्वप्रथम अहिंसा का अभ्यास करें,
मन-वचन-कर्म से अभ्यास करें।
सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करें।
सत्यमेव जयते ।
काम-ऊर्जा को आध्यात्मिक ओज में रूपान्तरित करें।
अस्तेय का पालन करें।
पर-सम्पत्ति के लोभी न बनें।
आन्तर-बाह्य शुचिता रखें।
सन्तोष का जीवन व्यतीत करें।
हृदय को शुद्ध करने के लिए तप करें।
धधकती अग्नि की तरह दमकें ।
स्वाध्याय करें और जप भी।
कर्म-फल भगवान् को समर्पित कर दें।
कर्तृत्व के अभिमान तथा कर्मफलाशा का त्याग करें।
स्व-इच्छा तथा वैश्व-इच्छा को एक हो जाने दें।
जागतिक उत्तरदायित्वों को भूल जायें और निश्चिन्त हो जायें ।
ईश्वर को अपना परम लक्ष्य मान कर
ध्यान के किसी आसन में बैठ जायें।
शिर- गरदन धड़ एक-सीध में रहें।
पद्मासन या सिद्धासन को सिद्ध कर लें।
चट्टान की तरह निश्चल बैठें।
शरीर स्थिर रहे।
शरीर मन का साँचा है।
शरीर हिलेगा, तो मन भी हिलेगा।
कपड़े, व्याघ्रचर्म तथा कुशासन पर बैठे।
अपने श्वास-प्रश्वास का नियमन करें।
रेचक, कुम्भक तथा पूरक का अभ्यास करें।
कुम्भक करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें।
इस प्रकार नाड़ियों को शुद्ध करें और मन को स्थिर करें।
अब इन्द्रियों के परावर्तन की बात करें।
इसी को प्रत्याहार कहते हैं।
इससे बहिर्मुखी इन्द्रियाँ नियन्त्रित होती हैं।
और वे अपने-अपने गोलकों के बाहर नहीं जाने पातीं।
लक्ष्य पर मन को एकाग्र करें।
यही धारणा है (जो ध्यान से पूर्व की अवस्था है)।
ईश्वर के एकमात्र विचार को ही निरन्तर प्रवाहित होने दें।
यह ध्यान है।
धारणा की स्थिति में सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।
वे बाधाएँ हैं, अतः उनकी उपेक्षा करें।
असीम परमानन्द के आकाश में उड़ान भरें
और कैवल्य तथा परम स्वतन्त्रता प्राप्त करें।
गहन ध्यान के उपरान्त आप समाधि-अवस्था में प्रवेश करते हैं।
समाधि परम चेतना की अवस्था है जो संस्कारों को नष्ट करती है।
समाधि से प्राप्त होते हैं प्रबोधन तथा परमानन्द ।
समाधि मुक्त करती है साधक को जन्म-मृत्यु के चक्र से।
२. योग के अंग तथा लक्ष्य
यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि-
ये हैं योग के अंग ।
आन्तरिक यौगिक जीवन का प्रारम्भ धारणा है।
ध्यान मध्यमावस्था है ।
चरमावस्था है समाधि ।
धारणा की निरन्तरता ही ध्यान है।
समाधि योग की पूर्णता तथा पराकाष्ठा है।
समाधि है ध्यान का फल ।
जब आप ॐ का सस्वर उच्चारण करते हैं,
तब सभी ध्वनियाँ ॐ के नाद में डूब जाती हैं।
इसी प्रकार जब आप ब्रह्माकार-वृत्ति को उत्पन्न करते हैं,
तब समस्त ऐन्द्रिय वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं।
वे एकमात्र ब्रह्माकार-वृत्ति से एकाकार हो जाती हैं।
३. धारणा
वास्तविक राजयोग का प्रारम्भ धारणा से होता है।
किसी बिन्दु पर मन को एकाग्र करना धारणा है।
धारणा ध्यान में विलीन हो जाती है।
धारणा ध्यान का एक अंग है।
धारणा का अन्त ध्यान में होता है।
ध्यान का अन्त समाधि में होता है।
यह बतलाना कठिन है कि
प्रत्याहार का अन्त कहाँ होता है?
और धारणा कहाँ प्रारम्भ होती है?
जहाँ धारणा समाप्त होती है,
वहाँ ध्यान का प्रारम्भ होता है।
एकाग्रता, ध्यान, समाधि मिल कर 'संयम' बनते हैं।
बीस सेकण्ड तक किया गया धारणा का अभ्यास
एक ध्यान के बराबर होता है।
इस प्रकार के बीस ध्यान
एक समाधि के बराबर होते हैं।
यह सूत्र प्रारम्भिक अभ्यासियों के लिए है।
४. धारणा (एकाग्रता) की शक्ति
यदि आप (आतशी) शीशे से सूर्य की किरणों को संकेन्द्रित करें,
तो ये किरणें रुई या कागज को भस्मीभूत कर देंगी।
परन्तु छितरी हुई किरणें, जो संकेन्द्रित न हों,
ऐसा नहीं कर सकतीं।
जब आप दूर खड़े किसी व्यक्ति से वार्तालाप करना चाहते हैं,
तब आप अपनी दोनों हथेलियों को
छुच्छी (कीप) की तरह बना लेते हैं और बोलते हैं।
उस समय आपके स्वर की लहरियाँ
एक ही स्थान पर एकत्र हो जाती हैं,
और उस व्यक्ति की ओर चल पड़ती हैं।
तब वह व्यक्ति आपके स्वर को साफ-साफ सुन पाता है।
पानी से भाप बनती है
और भाप का रूपान्तरण ऊर्जा के एक ऐसे बिन्दु में होता है,
जो शक्तिशाली रेल इंजन तक में गति उत्पन्न कर देता है।
आग पर चढ़े हुए बरतन की भाप
ढक्कन में गति उत्पन्न कर देती है।
ये संकेन्द्रित तरंगों के उदाहरण हैं।
इसी प्रकार जब मन की बिखरी हुई वृत्तियों को एकत्र करके
एक बिन्दु पर संकेन्द्रित कर लेते हैं.
तो आपकी एकाग्रता निश्चित ही अत्युत्तम बन जाती है।
एकाग्र मन एक शक्तिशाली सर्चलाईट की तरह बन जाता है
और आत्मा की छिपी हुई सम्पत्ति को
खोजने में आपकी सहायता करता है।
तब आप आत्मा के परम धन
शाश्वत परमानन्द, अमरता तथा
चिरस्थायी आनन्द को प्राप्त कर लेते हैं।
अतः धारणा और ध्यान का नियमित अभ्यास करें।
५. धारणा के सहायक साधन
कुम्भक से धारणा का अभ्यास करने में सहायता मिलती है।
यह मन की चंचलता को समाप्त करता है।
कुम्भक से मन के वृत्ति-मण्डल छोटे-छोटे हो जाते हैं
और अन्ततः इसकी भटकन पूर्णतः नियन्त्रित हो जाती है।
मोमबत्ती की लौ या किसी काले बिन्दु पर,
अथवा शिवलिंग या शालिग्राम पर,
मन को एकाग्र करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य भी धारणा के अभ्यास में सहायक होता है।
इसके बिना धारणा के अभ्यास में सुनिश्चित सफलता नहीं मिल सकती।
सात्त्विक भोजन एक अन्य साधन है।
एकान्त-वास, मौन, सत्संग, आसन-जय,
यम-नियम का पालन, उपवास,
मिताहार, असंगता,
अल्प वार्ता, अल्प आयास, अल्प चलन-
ये सब धारणा के सहायक साधन हैं।
६. धारणा में अध्यवसाय
अधीर व्यक्ति धारणा का अभ्यास नहीं कर सकता।
वह कुछ ही क्षणों के पश्चात् अपना आसन छोड़ कर उठ खड़ा होगा।
वह एक सप्ताह या माह के अन्दर ही अपना अभ्यास छोड़ देगा।
एकाग्रता के लिए गर्दभवत् अध्यवसाय की आवश्यकता होती है।
प्रारम्भ में अध्यवसाय अत्यन्त अरुचिकर तथा क्लान्तिकर प्रतीत होता है,
क्योंकि इसमें मनस-ऊर्मियों को ऊर्ध्वगामी बनाना होता है।
यह कुछ वैसा ही है जैसे गंगा के जल को आप
बदरीनारायण की ओर ले जायें।
परन्तु बाद में धारणा शान्ति और परमानन्द प्रदान करती है।
किसी मेडिकल छात्र के लिए,
किसी घाव की मरहम-पट्टी करते समय पीप साफ करना घृणित कार्य होता है
परन्तु जब वह शल्य-चिकित्सक बन जाता है,
तब वह नित्य ही प्रसन्नता के साथ शल्य-चिकित्सा करता है।
एक डाक्टर को एक रोग के उपचार का पता लगाने के लिए
सहस्रों बार प्रयोग करना पड़ता था।
एक पक्षी ने घास के एक तिनके से समुद्र को खाली करने का प्रयत्न किया था।
उनकी तरह अध्यवसायी बनें।
केवल तभी योग में सफलता प्राप्त हो पायेगी।
७. एकाग्रता के पदार्थ
(१)
आप मोमबत्ती की लौ,
दीवाल में बना काला बिन्दु,
भोर का तारा,
सूर्यास्त, चन्द्रमा, तारक गण,
गंगा की ध्वनि,
अनाहत की ध्वनियाँ,
शरीर में स्थित कोई भी चक्र,
मूर्तियाँ ।
निर्गुण ब्रह्म ।
अमूर्त विचार जैसे-
परमानन्द, शान्ति, शुचिता, पूर्णता,
स्वतन्त्रता, मुक्ति, मन्त्र - ध्वनियाँ ।
नासिका में 'सोऽहं' श्वास-प्रश्वास,
नीला आकाश,
सर्वव्यापी वायु, प्रकाश, शून्यता,
हृदय-प्रदेश में दिखायी पड़ने वाला देदीप्यमान प्रकाश,
सात्त्विक, दिव्य स्वप्न-चित्र,
सन्तों के रूप,
'तत्-त्वम्-असि' की तरह के महावाक्य,
ॐ का प्रतीक
ॐ की अर्थवत्ता
अपने गुरु का रूप तथा उनके गुरु दिव्य गुण
या कोई भी रुचिकर वस्तु—
इनमें से किसी पर भी आप मन को एकाग्र कर सकते हैं।
(२)
विभिन्न पदार्थों पर एकाग्रता का अभ्यास करें।
इस प्रकार आपका मन अपूर्व रीति से प्रशिक्षित तथा अनुशासित हो जायेगा।
पहले मन को एकाग्र करें-
एक विशालकाय पदार्थ - हिमालय पर ।
फिर इसे एकाग्र करें एक सूक्ष्म पदार्थ-सरसों के दाने या आलपिन की नोक पर ।
इसके बाद किसी दूरस्थ पदार्थ पर,
फिर किसी निकटस्थ पदार्थ पर,
फिर किसी रंग, ध्वनि, स्पर्श, गन्ध या स्वाद पर,
फिर घड़ी की टिक-टिक पर,
इसके बाद सदाचार तथा करुणा पर,
तब 'ज्योतिषां तज्ज्योतिः' श्लोक पर,
फिर 'सत्यं, ज्ञानं, अनन्तम्' पर,
फिर विराट् पुरुष पर,
फिर हिरण्यगर्भ पर,
फिर भगवान् शिव की मूर्ति पर,
और तब 'अहं ब्रह्मास्मि' महावाक्य पर
मन को एकाग्र करें।
८. एकाग्रता से लाभ
एकाग्रता से वैज्ञानिकों तथा प्राचार्यों को
शोध-कार्य करने में सफलता मिलती है।
इससे डाक्टरों और वकीलों को अधिक कार्य करने में सहायता मिलती है।
इससे इच्छा-शक्ति विकसित होती है,
स्मरण-शक्ति प्रखर होती है।
बुद्धि प्रखर तथा प्रोज्ज्वल बनती है।
एकाग्रता, मानसिक शान्ति अथवा गाम्भीर्य,
आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति, धैर्य,
अधिक कार्य करने की क्षमता,
स्फूर्ति, कुशाग्र बुद्धि, सुरीला स्वर,
दीप्त नेत्र, सशक्त स्वर तथा वाणी,
दूसरों को प्रभावित तथा आकर्षित करने की शक्ति,
प्रफुल्लता, प्रसन्नता, आत्मानन्द तथा परम शान्ति प्रदान करती है।
यह अशान्ति, मानसिक उत्तेजना तथा आलस्य दूर करती है।
यह आपको निर्भीक तथा अनासक्त बनाती है।
यह आपको ब्रह्म-साक्षात्कार करने में सहायता प्रदान करती है।
९. ध्यान
(१)
'ध्यानं निर्विषयं मनः'
समस्त पदार्थों तथा ऐन्द्रिक सुखों के चिन्तन से
मन को मुक्त रखना ध्यान है।
यदि ऐसा सम्भव हो सका,
तो ब्रह्म-साक्षात्कार स्वतः ही घटित होगा;
भगवान् आपके मन-मन्दिर में आ विराजेगा;
ध्यान बिना किसी प्रयास के ही होने लगेगा।
यदि आप किसी अँधेरी गुफा-
सहस्रों वर्षों से अँधेरे की कारा में बन्द गुफा–में प्रकाश ले आयें,
तो अन्धकार क्षण-भर में विलीन हो जायेगा।
अन्धकार को हटाने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना होगा।
कूड़ा-कर्कट से भरे किसी पात्र में
आप हाथ डालना चाहें,
तो नहीं डाल पायेंगे।
पात्र को खाली कर दें।
अब हाथ डालने में क्या कठिनाई है!
इसी प्रकार मन के पात्र से भी विषयों का कूड़ा-कर्कट निकाल दें।
पलक झपकते ही ईश्वर उसमें प्रवेश कर जायेगा ।
(२)
कोई आवश्यक कार्य तुरन्त कर डालने की बात मन में हो,
तो ध्यान के लिए न बैठें,
नहीं तो मन अशान्त हो जायेगा
और बार-बार उस कार्य के बारे में ही सोचेगा ।
आप मन को एकाग्र न कर पायेंगे।
नित्य ही दिव्य जीवन व्यतीत करें।
दिव्यता को अपने जीवन में अभिव्यक्त होने दें।
तभी ध्यान फलित होगा।
गंगा तट पर या मन्दिर में बैठें।
ऐसे स्थानों में ध्यान अच्छा लगेगा।
ध्यान प्रारम्भ करने से पूर्व-
गुरु-स्तोत्र का पाठ करें,
शान्ति-पाठ करें,
या प्रार्थनाएँ कहें।
सहिष्णु, अनासक्त, अध्यवसायी, निर्भीक, बुद्धिमान् तथा पवित्र बनें।
आपको ध्यान में सफलता मिलेगी।
आप निर्विकल्प-समाधि की अवस्था-
जिसमें सारे विचार नष्ट हो जाते हैं-
में प्रवेश करेंगे।
(३)
पहले गणपति गणेश तथा अपने गुरु को प्रणाम करें।
अपने 'भूत' को भूल जायें ।
ध्यान करते समय पुरानी स्मृतियाँ आपको अशान्त बना देंगी।
तटस्थ बन जायें।
ध्यान के पदार्थ का चिन्तन करें।
भावनाओं तथा आवेगों पर नियन्त्रण प्राप्त करें।
धैर्य रखें।
जब पैरों में पीड़ा होने लगे,
तब जल्दी ही उठ कर खड़े न हो जाये।
दृढ़ बना रहें।
अभ्यास में रत रहें।
साहसी बनें।
किसी एकान्त स्थान में बैठे और ध्यान करें।
हवाई महल बनाना छोड़ दें,
योजनाएँ भी न बनायें।
तन्द्रा और निद्रा को कुम्भक के अभ्यास तथा
कीर्तन की सहायता से भगा दें।
पहले मन की वृत्तियों के मण्डल को छोटा करें।
जैसे-जैसे मण्डल छोटा होता जायेगा,
मन केन्द्रित होने लगेगा।
जब यह केन्द्रित हो जाये,
तब इसे विक्षुब्ध न करें।
इसे पुरानी लीकों पर न चलने दें।
१०. नियमित ध्यान करें
सन्तुष्ट, प्रसन्न तथा शान्त रहें
केवल तभी आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं।
उत्तेजित या व्याकुल मन हो,
तो ध्यान नहीं किया जा सकता।
किसी व्यक्ति के प्रति अपने मन में शिकायत न रखें।
जो आपकी निन्दा करे, उसे क्षमा करें।
उस पर तरस खायें;
और कहें वह एक अज्ञानी, अविकसित आत्मा है।
कभी-कभी मन को फुसलायें-
जिस प्रकार आप बच्चे को फुसलाते हैं।
कभी-कभी इसका उपहास करें।
इसे लज्जित भी करें।
कभी-कभी इसका निरोध भी करें।
परन्तु इसके साथ जोर-जबरदस्ती न करें।
इस प्रकार मन को चतुराई तथा व्यवहार कुशलता से नियन्त्रित करें।
शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।
११. चार प्रकार के ध्यान
चार प्रकार के ध्यान होते हैं-
स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम ।
सवितर्क तथा निर्वितर्क ध्यान स्थूल ध्यान हैं।
सविचार तथा निर्विचार ध्यान सूक्ष्म ध्यान हैं।
सानन्द ध्यान सूक्ष्मतर ध्यान है।
सस्मित ध्यान सूक्ष्मतम ध्यान है।
शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए
भगवान् विष्णु पर ध्यान स्थूल ध्यान है।
सद्गुणों पर ध्यान सूक्ष्म ध्यान है।
प्रकाश पर ध्यान भी सूक्ष्म ध्यान है।
सुन्दरता, परमानन्द, शान्ति का ध्यान सूक्ष्मतर ध्यान है।
निराकार ब्रह्म का ध्यान सूक्ष्मतम ध्यान है।
स्थूल ध्यान मूर्त ध्यान है।
सूक्ष्म ध्यान अमूर्त ध्यान है।
१२. प्रतिलोमी प्रक्रिया
कारण का ध्यान करें ।
कार्य को नकारें।
कारण-रूप पंचतत्त्वों के कार्य पदार्थ हैं।
कारण-रूप प्रकृति के कार्य पंचतत्त्व हैं।
इस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म की ओर जायें।
यह प्रक्रिया आपको उस ब्रह्म की ओर ले जायेगी
जो प्रत्येक वस्तु का कारण रहित कारण है।
यह ध्यान का एक प्रभावशाली उपाय है।
१३. विचार
यह शरीर पंचतत्त्वों से निर्मित है।
अब निम्नांकित विचार - बिन्दुओं की कल्पना करें,
इनका ध्यान करें तथा अनुभव करें :
इस शरीर का पृथ्वी- अंश
पृथ्वी तत्त्व में विलीन हो जाता है।
शरीर का जलीय अंश अपस् तत्त्व में,
अग्निमय अंश तेजस् में,
वायवीय अंश वायु-तत्त्व में,
आकाश अंश आकाश-तत्त्व में
तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार
मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं।
शेष क्या बचता है?
आपकी अपनी आत्मा ही शेष बचती है—
जो है सर्वव्यापक तथा अमर । हे राम !
तत् त्वम् असि ।
इसका अनुभव करें।
इसका साक्षात्कार करें
तथा मुक्त हो जायें।
१४. सद्गुणों का ध्यान
साहस, आत्म-संयम, न्याय,
सत्यता, अहिंसा, शुचिता, दया,
विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य-
ये सब महत्त्वपूर्ण सद्गुण हैं।
परोपकारिता, दानशीलता, उदारता-
ये अन्य सद्गुण हैं।
इन सद्गुणों का निरन्तर ध्यान करें।
इन सद्गुणों से प्राप्त होने वाले लाभों का चिन्तन करें।
दुर्गुणों को नष्ट करें।
आपमें उपर्युक्त सद्गुण विकसित होंगे।
समस्त वस्तुओं के स्रोत आत्मा पर अविरत ध्यान करें।
इन सद्गुणों के आगार
अनन्त कल्याणकारी गुणों के आकर
भगवान् पर ध्यान करें।
आपमें समस्त सद्गुणों का विकास होगा।
१५. ध्यानयोग (सगुण)
ध्यान के किसी आसन में स्थिर बैठें।
शिर, ग्रीवा तथा धड़ एक सीध में रहें।
शरीर को हिलायें नहीं ।
मूर्ति की तरह स्थिर रहें ।
अभ्यास करते-करते तीन घण्टों तक बैठें।
ब्राह्ममुहूर्त में ध्यानाभ्यास करें।
आँखें बन्द कर लें
और त्रिकुटी या हृदय पर ध्यान करें।
योगी जन त्रिकुटी पर मन को एकाग्र करते हैं तथा
भक्त साधक हृदय पर ।
भगवान् के चित्र का मानस-दर्शन करें।
मन को उनके पैरों से शिर तक ले जायें।
पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठें।
पद्मासन या सिद्धासन में बैठें।
सुखासन में भी बैठ सकते हैं।
प्रारम्भ में कुछ प्रार्थनाएँ गायें ।
नित्य दो या तीन बार बैठें।
जाड़े में उग्र साधना करें।
एकाग्रता (धारणा) के बाद ध्यान की स्थिति आती है।
ध्यान के बाद समाधि की स्थिति आती है।
भगवन्नाम का जप करें।
भगवान् के गुणों का चिन्तन करें।
उनकी लीलाओं का चिन्तन करें।
इससे आपका ध्यान प्रभावकारी बनेगा।
लक्ष्य पर बार-बार मन को लायें।
ध्यानाभ्यास करते समय धैर्य रखें।
तभी आपको सफलता मिलेगी।
ध्यान से सांसारिक विचार अवरुद्ध हो जाते हैं।
ध्यान से सत्त्वगुण में वृद्धि होती है।
ध्यान से साधक का स्वास्थ्य सुन्दर बनता है।
ध्यान से साधक दिव्य बनता है।
ध्यान पीड़ा और शोक का हरण करता है।
ध्यान पुनर्जन्मों से मुक्त करता है।
ध्यान शान्ति और परमानन्द प्रदान करता है।
अतः नियमित ध्यान करें।
१६. ध्यानयोग (निर्गुण)
यह उस ब्रह्म का ध्यान है—
जो अद्वैत तथा निर्गुण है; जो आत्म-प्रदीप्त तथा अविभाज्य है:
जो शुचि तथा निर्विकार है।
पहले नेति नेति के सिद्धान्त का अभ्यास करें।
प्रातिभासिक उपाधियों को नकारें।
मन, प्राण और शरीर का उदात्तीकरण करें।
कोशों को अनात्म समझ कर उतार फेंकें।
जिस प्रकार आप घास से असार तत्त्व हटा कर
उसका सारतत्त्व ले लेते हैं,
और दूध से मक्खन निकाल लेते हैं,
उसी प्रकार ध्यान के मन्थन से ब्रह्म-रूपी सारतत्त्व को ग्रहण करें।
विचार करें -मैं कौन हैं ?
ध्यान करें— मैं सत्, चित्, आनन्द हूँ।
अनुभव करें— मैं साक्षी हूँ।
आत्मा से तादात्म्य स्थापित करें।
अनुभव करें मैं शरीर से पृथक् हूँ;
मैं कोशों से अलग हूँ;
मैं जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं का साक्षी हूँ;
मैं शाश्वत निराकार आत्मा हूँ।
मानसिक रूप से कहें-
भाव और भावना के साथ कहें- ॐ ॐ ॐ ।
अपनी श्वास के साथ 'सो' को सम्बद्ध करें
तथा प्रश्वास के साथ 'हं' को ।
'अहं ब्रह्मास्मि' महावाक्य
या 'शिवोऽहम्' सूत्र
का ध्यान करें तथा निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रवेश करें।
दृढ़तापूर्वक कहें, पहचानें तथा नमस्कार करें—
'मैं प्रकाशों का प्रकाश हूँ, ॐ ॐ ॐ ।'
'मैं अमर आत्मा हूँ, ॐ ॐ ॐ ।
'मैं चेतना हूँ, ॐ ॐ ॐ ।'
अनुभव करें— 'मैं कर्ता नहीं हूँ ।'
'मैं भोक्ता नहीं हूँ।'
'मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ।'
'मैं असंग हूँ।'
जप करें- "सोऽहम् शिवोऽहम्
अहं ब्रह्मास्मि
सच्चिदानन्द
स्वरूपोऽहम् ।”
"हंसः सोऽहम्, सोऽहम् हंसः ।
हंसः सोऽहम्, सोऽहम् हंसः ।
हंसः सोऽहम्, सोऽहम् हंसः ।
हंसः सोऽहम्, सोऽहम् हंसः । "
“ब्रह्मैवाहम्, ब्रह्मैवाहम्
ब्रह्मैवाहम्, ब्रह्मोऽहम् ;
शिवैवाहम्, शिवैवाहम्
शिवैवाहम् शिवोऽहम्।"
१७. भगवान् पर ध्यान
उस भगवान् का ध्यान करें,
जो आन्तरिक शासक है;
जो हमारे हृदयों में निवास करता है।
तब आपका हृदयकमल खिल उठेगा।
तब प्रज्ञा का सूर्य चमकने लगेगा।
हृदय का अन्धकार दूर हो जायेगा ।
पंचक्लेशों का नाश हो जायेगा ।
तीनों अग्नियाँ बुझ जायेंगी।
पाप और संस्कार
वासनाएँ और कामनाएँ
भस्मीभूत हो जायेंगी।
१८. शाश्वत तत्त्व का ध्यान
उस शाश्वत तत्त्व का ध्यान करें,
जो है मुक्त-
पापों, कलंकों, रोगों, भयों तथा विभ्रमों से ।
वह है—
सर्वव्यापक, शुचि, दूर होते हुए भी निकट,
पंचतत्त्वों का उद्गम स्थल,
योगियों और सन्तों का परम लक्ष्य तथा
मन, इन्द्रियों और वेदों का स्रोत ।
वहाँ परम शान्ति का,
विचारातीत परमानन्द का तथा
परम भव्य प्रकाश का वास है।
वहाँ विचार निष्क्रिय हो जाते हैं।
वहाँ सर्वव्यापक परम शान्ति का राज्य है।
वहाँ न रव है, द्वन्द्व ।
१९. ध्यान के पदार्थ
वेदान्त के विद्यार्थी भी
ध्यानाभ्यास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में
सर्वव्यापक आकाश तथा
ज्योति के महत्त्व को समझते हैं।
उन्हें बाह्य तत्त्वों से सहायता मिलती है।
भक्त जन
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य अथवा माधुर्य भाव से
अपने प्रेमास्पद का ध्यान करते हैं।
२०. ध्यान में अवरोध
(१)
ध्यान के चार मुख्य अवरोध हैं-
विषयासक्ति, मतिमन्दता,
कुतर्क१, '
विपरीत भावना।'२
इनमें से कोई अकेला भी
वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने में बाधक बन सकता है।
अतः वैराग्य भाव को पोषित करें।
अपनी बुद्धि को प्रखर करें।
कुतर्क और विपरीत भावना का त्याग करें।
शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करें।
आपको त्वरित आत्मज्ञान प्राप्त होगा।
------------------------------------------------
१ धर्मग्रन्थों की भ्रान्त व्याख्या ।
२ इस त्रुटिपूर्ण धारणा पर विश्वास कि आत्मा सुखी-दुःखी होती है।
(२)
मन ऐन्द्रिय पदार्थों का अनवरत चिन्तन करता है।
जब यह चिन्तन करते-करते थक जाता है,
तब यह सो जाता है और मूल अविद्या की स्थिति में विश्राम करता है।
ध्यान करते समय यदि आप-
निद्रा या लय के प्रभाव में आ जायें,
तो सतर्क हो कर मन को जगा दें।
यदि विक्षेप के कारण मन चंचल हो जाये,
तो इसे शान्त करें।
यदि मन किसी पदार्थ में आसक्त है,
तो उसे आसक्ति से मुक्त करें।
बार-बार ब्रह्म-चिन्तन करें।
पूर्ण उत्साह के साथ ब्रह्म-चिन्तन करना प्रारम्भ कर दें।
सविकल्प-समाधि के परमानन्द के भी प्रति उदासीन हो जायें।
यह परमानन्द भी सर्वोच्च साक्षात्कार में बाधक होता है।
जब मन पूर्णतः शान्त हो जाये,
तब इसे किंचित् भी क्षुब्ध न करें।
उत्साहपूर्वक ध्यान करते रहें ।
आप शीघ्र ही निर्विकल्प-समाधि की अवस्था में प्रवेश करके
चरम सार्वलौकिक परमानन्द का साक्षात्कार करेंगे।
२१. सतर्क रहें
यदि आप सतर्क नहीं हैं,
यदि आप ध्यानाभ्यास में नियमित नहीं हैं,
यदि आप ऐन्द्रिय सुखों से किंचित् भी प्रभावित हो जाते हैं,
तो मन अधोगामी बन जायेगा-
सीढ़ियों से लुढ़कते हुए गेंद की तरह ।
झील की सतह से नरकट विस्थापित होने पर
दोबारा तुरन्त ही आपस में मिल जाते हैं।
इसी प्रकार यदि साधक किंचित् समय के लिए भी
साधना और ध्यान का अभ्यास करना बन्द कर दे,
तो माया उसे तुरन्त अभिभूत कर लेती है।
अतः सावधान और सतर्क रहें।
अपने ध्यानाभ्यास में नियमित रहें।
२२. अवलोकन तथा विवेचन करें
जब मन सुस्त अथवा निद्रालु होने लगे,
तब कीर्तन, जप, प्रार्थना, प्राणायाम आदि करें।
सर्वांगासन, शीर्षासन, दीर्घकालीन प्रणवोच्चार आदि
की सहायता से इसे जाग्रत करें।
जब यह चंचल हो जाये,
तब एकान्त वास, जप, त्राटक, मौन आदि का अभ्यास करके,
दृढ़तापूर्वक तथा आसक्ति-रहित हो कर
इसे स्थिर, एकाग्र तथा शान्त करें।
जब यह आसक्त हो जाये,
तब वैराग्य, सतर्कता, दोषदृष्टि३, मिथ्यादृष्टि४ की सहायता से
इसे आसक्ति-रहित बनायें ।
जब यह नियन्त्रित हो जाये,
तब इसे और अधिक विक्षुब्ध न करें।
जब आपको सविकल्प-समाधि के परमानन्द का अनुभव होने लगे,
तब इसके प्रति आसक्त न हो जायें।
अवलोकन-विवेचन करें
तथा निर्विकल्प-समाधि की अवस्था में प्रवेश करने का प्रयत्न करें।
------------------------------------------------------------------
३ ऐन्द्रिय जीवन में दोष ढूँढना।
४ सब पदार्थ मिथ्या हैं—इस मान्यता को स्वीकार करना ।
२३. ध्यान तथा ज्ञान
ध्यान साधन है।
ज्ञान लक्ष्य है।
ध्यान प्रक्रिया है।
ज्ञान उसकी पूर्णता है।
ध्यान में प्रयास है।
ज्ञान में प्रयास नहीं है।
ध्यान की अवस्था में ध्याता साधक-मात्र ही रहता है।
ध्यान की अवस्था के उस पार
जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं,
तथा ध्याता सत्य का ज्ञाता बन जाता है और
जीवन्मुक्त हो जाता है।
जब आप किसी वृक्ष को देखने का प्रयत्न करते हैं,
तब प्रारम्भ में देखने की क्रिया में 'आयास' की क्रिया सन्निहित रहती है।
बाद में यह क्रिया वृक्ष की चेतना के अनवरत प्रवाह में रूपान्तरित हो जाती है।
ब्रह्मज्ञान भी इसी प्रकार का होता है।
प्रारम्भ में प्रयास किया जाता है।
बाद में साधक ध्येय में विलीन हो जाता है।
तब किसी प्रकार का आयास नहीं रह जाता।
२४. समाधि
समाधि है परमानन्द से परिपूर्ण मिलन ।
इस अवस्था में जीव का ब्रह्म से मिलन होता है।
तृतीय नेत्र खुल जाता है।
इन्द्रियों का निग्रह हो जाता है।
चंचल मन शान्त हो जाता है।
नाम-रूप की सत्ता समाप्त हो जाती है।
केवल ब्रह्म ही प्रकाशमान रहता है
समाधिस्थ योगी अपनी वासनाओं को नष्ट कर देता है,
अपने विचारों पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है,
अपनी कामनाओं को दमित कर डालता है,
मोह पापों को नष्ट कर देता है,
अपनी अहंमन्यता को समाप्त कर देता है,
रुचि अरुचि की भावनाओं से मुक्त हो जाता है।
वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है।
वह दिव्यामृत का पान करता है, अमर हो जाता है,
अपनी आत्मा में ही रमण करके सुख प्राप्त करता है,
सर्वत्र अपनी आत्मा को ही देखता
वह अहंभाव तथा दुःखों से मुक्त हो जाता है,
प्रकाश स्तम्भ की तरह वह चमकता है।
उसकी प्रसन्नता चारों ओर विकिरित होती है।
२५. संस्कार - शेष
संस्कारों का अर्थ है कर्मों की छाप ।
शेष का अर्थ हैं अवशिष्ट ।
संस्कार - शेष का अर्थ हुआ कर्मों की अवशिष्ट छाप ।
सवितर्क, सविचार,
निर्वितर्क, निर्विचार,
सानन्द, सस्मिता
समाधियों की अवस्था में रहने वाले राजयोगी की सविकल्प-समाधि
छोड़ती है (अवशिष्ट) छाप 'अहमस्मि' की।
यह संस्कार - शेष कहलाता है।
यह मुनियों की लेश- अविद्या के अनुरूप होता है।
जीवन्मुक्ति की स्थिति उपलब्ध कर लेने के पश्चात् भी
साधक में अविद्या का अवशेष रह जाता है,
जिसका वह अनुभव करता रहता है।
इसी के कारण वह विचरण करता है,
स्नान करता है, मल-मूत्र त्याग करता है,
भोजन करता है, पानी पीता है।
लेश- अविद्या का प्रभाव होता है—
लहसुन की उस गन्ध की तरह
जो पात्र को साफ करने के बाद भी उससे आती रहती है।
२६. मन समाधि में विगलित हो जाता है
कर्पूर अग्नि में पिघलता है
और फिर अग्नि का ही रूप ग्रहण कर लेता है।
जब नमक पानी में घुल जाता है,
तब वह पानी से पृथक् नहीं दिखलायी देता ।
केवल पानी ही बच रहता है।
इसी प्रकार जब मन
ब्रह्म- जो अद्वैत है—का रूप ग्रहण कर लेता है,
तब मन नहीं दिखायी पड़ता ।
तब एकमात्र ब्रह्म ही अपनी आद्य महिमा में अवस्थित रहता है।
२७. निर्विकल्प-समाधि
(१)
निर्विकल्प समाधि में
अहं की चेतना विद्यमान नहीं रहती।
अहंभाव तथा मन ब्रह्म के साथ मिल कर एक हो जाते हैं।
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी
सम्पूर्णतः विलीन हो जाती है।
शुद्ध मन ब्रह्म का रूप ग्रहण कर लेता है।
यही अवस्था असम्प्रज्ञात, निरालम्ब या निर्बीज-समाधि कहलाती है।
इस अवस्था में मन के लिए कोई अवलम्ब नहीं रहता।
ब्रह्म अपनी ही महिमा में अवस्थित रहता है।
संस्कार पूर्णतः भस्मीभूत हो जाते हैं।
सविकल्प-समाधि
निर्विकल्प समाधि में रूपान्तरित हो कर और भी गहन बन जाती है।
निर्विकल्प समाधि में किसी भी प्रकार के विचारों का अस्तित्व नहीं होता।
यह परम चेतना की
एक विचार-रहित अवस्था है।
(२)
निर्विकल्प का अर्थ है-
विकल्प का अभाव ।
जो स्थिति किसी विचार से सम्बद्ध न हो,
वह है निर्विकल्प की स्थिति ।
निर्विकल्प समाधि की स्थिति में कोई भी विचार नहीं रहता।
न कल्पना-शक्ति सक्रिय रहती है और न बुद्धि या मन ।
समस्त वृत्तियाँ कार्य करना बन्द कर देती हैं।
उस समय केवल शुद्ध चेतना या जागरूकता की स्थिति होती है।
समस्त संस्कार तथा वासनाएँ पूर्णतः भस्मीभूत हो जाती हैं।
अहंभाव भी भस्मीभूत हो जाता है।
मनोभावों का संसार भी
जो सांसारिक प्राणियों के लिए भी अत्यन्त मोहक होता है।
भस्मीभूत हो जाता है।
समस्त नाम रूप भी भस्मीभूत हो जाते हैं।
केवल बच रहता है अस्ति-भाति-प्रिय ।
अस्ति भाति प्रिय सत्-चित्-आनन्द ।
जिसका अस्तित्व सदैव रहे, वह है अस्ति ।
जो चमके, वह है भाति ।
यह परम चेतना है।
जो प्रसन्नता दे, वह प्रिय है।
यह विशुद्ध अमर आनन्द है ।
निर्विकल्प - समाधि की अवस्था में
मन विक्षेपों, आसक्तियों,
आलस्य तथा अन्य विकारों से मुक्त रहता है।
यह दीपक की उस लौ की तरह स्थिर जो जाता है,
जो वायु के थपेड़ों से सुरक्षित रहती है।
(३)
निर्विकल्प समाधि विचारातीत अवस्था है।
इसमें सारे द्वित्व नष्ट हो जाते हैं,
परम शुद्ध चेतना की सत्ता रहती है तथा ।
रहता है पूर्ण बोध
किसी प्रकार की कामना या अहंमन्यता भी नहीं रहती।
समाधिस्थ योगी के परमानन्द का पारावार नहीं रहता।
वह अनन्त सत्ता से एकाकार हो जाता है।
वह स्वच्छन्द, पूर्ण तथा स्वतन्त्र होता है।
वह आप्तकाम होता है।
उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है।
वह परम शान्ति को प्राप्त होता है।
२८. रहस्यवाद
रहस्यवाद है अन्तर्प्रज्ञावाद ।
रहस्यवाद है मनसातीतत्व ।
रहस्यवाद है अपरोक्ष अनुभूति ।
रहस्यवाद है प्रत्यक्ष आत्म-साक्षात्कार ।
रहस्यवाद है अनुभव अद्वैत ।
रहस्यवाद है आध्यात्मिक, अन्तर्ज्ञात अनुभव
जो बुद्धिगम्य नहीं है।
रहस्यवाद है निर्विकल्प-समाधि ।
रहस्यवाद है ईश्वर से सीधा सम्पर्क ।
रहस्यवादी रहस्यवाद में निष्णात होता है।
२९. सब-कुछ है अखण्ड एकरस स्वरूप
परब्रह्म है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
गुरु है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
शिष्य है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
जीव है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
साक्षी है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
अग्नि है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
जल है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
वायु है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
आकाश है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
मन है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
बुद्धि है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
नेत्र है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
यह संसार है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
सब कुछ है अखण्ड एकरस स्वरूप ।
३०. विलयन
जब आप ब्रह्म के साथ एकता का साक्षात्कार कर लेते हैं,
जब आप प्रत्येक स्थान पर अद्वैत ब्रह्म का दर्शन करने लगते हैं।
तब 'यहाँ', 'वहाँ',
'यह', 'वह', 'मैं', 'तुम' या 'वह'
का प्रश्न कहाँ रह जाता है?
तब केवल एक ही समरूप परमानन्दपूर्ण सारतत्त्व का अस्तित्व रहता है।
तब केवल भूमा या अनन्त की सत्ता होती है।
समस्त प्रकार के द्वित्व, विभेद, अन्तर समाप्त हो जाते हैं।
द्रष्टा तथा दृश्य एक हो जाते हैं।
ज्ञाता तथा ध्येय एक हो जाते हैं। विचारक तथा विचार एक हो जाते हैं।
ज्ञाता तथा ज्ञेय एक हो जाते हैं।
यह अन्यूनता, पूर्णता, स्वतन्त्रता तथा चिरस्थायी आनन्द का
एक समग्र भावातीत अनुभव है।
३१. आध्यात्मिक अनुभव
(१)
अधिकाधिक वैराग्य और विवेक की प्रवृत्ति;
मोक्ष की अधिकाधिक आकांक्षा;
शान्ति, प्रसन्नता, सन्तोष;
निर्भीकता, अक्षुब्ध मन;
चमकीले नेत्र, सुवासित शरीर;
सुन्दर रूप-रंग, मधुर तथा प्रभावोत्पादक वाणी;
सुन्दर स्वास्थ्य, उत्साह, ओजस्विता तथा तेजस्विता,
रोग, आलस्य तथा विषाद से मुक्ति;
शरीर का हलकापन, मन की सतर्कता, सशक्त जठराग्नि;
लम्बे समय तक ध्यानाभ्यास करने हेतु बैठने की इच्छा;
सांसारिक वार्तालाप तथा सांसारिक प्राणियों का संग करने के प्रति अरुचि;
यह अनुभव करना कि — ईश्वर सर्वव्यापक है,
सभी प्राणी भगवान् के ही रूप हैं तथा
समस्त विश्व स्वयं भगवान् ही है;
सब प्राणियों के प्रति प्रेम-भाव
सभी प्राणियों के प्रति-
यहाँ तक कि निन्दकों के प्रति भी-
घृणा का अभाव,
अपमान आघात सहन करने की तथा
संकटों एवं विपत्तियों का सामना करने की मानसिक क्षमता
विसर्जित मल-मूत्र की मात्रा में कमी-
ये हैं कुछ प्राथमिक आध्यात्मिक अनुभव ।
ये इस तथ्य के संकेतक हैं-
आप अध्यात्म मार्ग पर स्थिर गति से आगे बढ़ रहे हैं।
(२)
ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होते हुए सफेद और रंगीन प्रकाश के गोले;
सूर्य तथा तारक गण;
दिव्य गन्ध, दिव्य स्वाद;
स्वप्न में भगवद्-दर्शन;
असाधारण, अतिमानवीय अनुभव;
मानव-रूप में—
कभी ब्राह्मण, कभी वृद्ध व्यक्ति, कभी कुष्ठी,
कभी चिथड़ों में लिपटे अछूत के रूप में-
भगवद्-दर्शन;
भगवान् से वार्तालाप-
ये हैं कुछ प्राथमिक आध्यात्मिक अनुभव ।
इसके बाद उस सविकल्प-समाधि
या वैश्व चेतना की स्थिति आती है।
जिसका अनुभव अर्जुन ने किया था।
अन्ततः साधक प्रवेश करता है
निर्विकल्प - समाधि की अवस्था में,
जिसमें न दृश्य रह जाता है और न द्रष्टा ;
जिसमें न कुछ दिखायी पड़ता है, न सुनायी पड़ता है।
इस अवस्था में साधक शाश्वत तत्त्व से एकाकार हो जाता है।
३२. मैं अमृत-पान करता हूँ
मेरे सद्गुरु ने मुझे प्रज्ञा की तलवार दी।
उन्होंने परम तत्त्व से मेरा योग करा दिया।
उन्होंने मेरे पतन गर्त तथा फन्दों को दूर किया ।
मैंने निर्विकार आनन्द की चरम स्थिति का साक्षात्कार किया।
इस स्थिति में
द्रष्टा और दृश्य लुप्त हो जाते हैं।
मेरे लिए अब और कुछ जानना शेष नहीं है।
मैं प्रत्येक स्थान पर पूर्णता की स्थिति में रहता हूँ।
जन्म- रोग से मैं मुक्त हो गया हूँ।
मैं अपने 'मैं' से मुक्त हो गया हूँ।
मैं परमानन्द का पुंज बन गया हूँ।
मैं अनश्वरता का अमृत पान करता हूँ।
यह अमृत समस्त मधुर पेयों से अधिक मधुर है।
३३. जहाँ वाणी की पहुँच नहीं है
पूर्ण, नाम-रहित निराकार शून्यता की स्थिति में,
असीम परमानन्द के विस्तार में,
मनसातीत तथा विषयातीत आनन्द के क्षेत्र में,
दिक्काल से मुक्त नीरवता के अनन्त धाम में,
मधुर सामंजस्य के भावातीत आवास में,
मैं परम दीप्ति से एकाकार हो गया।
द्वित्व और अनेकत्व का भाव समाप्त हो गया।
मैंने जन्म के सागर को सदा-सर्वदा के लिए पार कर लिया।
यह कृपा है गोवर्धनधारी, वृन्दावनविहारी भगवान् कृष्ण की।
३४. वह उच्च स्थिति
हिमालय की गुहा कन्दराओं में भगवान् को ढूँढ़ा था।
तीर्थों में ढूँढ़ा था।
सरिताओं के तटों पर ढूँढ़ा था ।
परन्तु अब मैं स्वयं ब्रह्म हूँ; देवों का देव हूँ।
एक समय था जब मुझे अपने घर से,
गाँव से, जिले से, प्रान्त से असीम प्यार था।
परन्तु अब तो मैं समस्त संसारों का घर हूँ।
मेरी दृष्टि में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
ग्रीस, भारत, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, रूस-
सब मिल कर एक हो गये हैं।
कभी मैं तमिल भाषा को प्यार करता था,
परन्तु अब तो मैं स्वयं 'ॐ' हूँ -
जो समस्त भाषाओं का स्रोत है।
कभी मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता था,
परन्तु अब मैंने साक्षात्कार कर लिया है इस तथ्य का
कि समस्त शरीर मेरे हैं।
कभी मेरे लिए सौ वर्षों की अवधि एक लम्बी अवधि थी,
परन्तु अब मैं शाश्वतत्व में निवास करता हूँ।
अब मुझे पंचांग-पत्रा की, घड़ी की आवश्यकता नहीं है।
कभी मेरे लिए पाँच हजार मील की दूरी बहुत बड़ी दूरी थी,
परन्तु अब मैं अनुभव करता हूँ कि मैं अनन्त हूँ।
मेरे लिए दिक्काल की सीमाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है।
मेरा न कोई घर है, न नाम और न पता ।
३५. मैं नीरवता में निवास करता हूँ
संसार मुझे बुरा कहे या भला-
मुझे आलोचना की चिन्ता नहीं है।
क्यों करूँ चिन्ता मैं ?
मेरा आवास है लोकोत्तर ।
मैं शुभ-अशुभ से, प्रशंसा-निन्दा से परे हूँ।
शरीर-मन से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।
मुझे न भय है और न किसी से अपेक्षा है।
मुझे इस संसार से क्या लेना-देना है।
मैं ब्रह्मानन्द के सागर में तैर रहा हूँ।
मैं किसी व्यक्ति का अनुग्रह या संस्तुति नहीं चाहता ।
मैं किसी व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं करना चाहता।
मुझे किसी व्यक्ति की सहायता या संगति की आवश्यकता नहीं है।
मैं नीरवता में निवास करता हूँ।
नीरवता में आनन्दित होता हूँ।
मैं स्वयं नीरवता हूँ।
हे शिष्यो ! शिष्यो !! सभी मित्र गण मुझे सुनें!!!
मुझे अब छोड़ दें। मैं आपसे विदा लेता हूँ।
३६. मैं अब परमानन्दमय हूँ
मैंने घर-बार छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया है,
सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दिया है।
संसार की निरर्थकता और ओछेपन को भी मैंने खूब समझ लिया है।
पदार्थों की निस्सारता को भी समझ लिया है।
कामुकता, क्रोध, दम्भ का भी परित्याग कर दिया है।
पदार्थों को प्राप्त करने की कामना पर भी मैंने विजय प्राप्त कर ली है।
हिमालय में गंगा तट पर मैं बैठा।
मनन किया।
ब्रह्म-चिन्तन किया।
अज्ञान नष्ट हो गया।
हृदय से तृष्णाएँ निकल गयीं।
बोझिल हृदय तृष्णाओं के भार से मुक्त हुआ ।
अब मेरे अन्दर पवित्रता और शान्ति हैं।
मैं बिलकुल शान्त हूँ-
अनुभव करता हूँ शाश्वतत्व की परम शान्ति को ।
परमानन्दमय हो गया हूँ अब, और
पहचान लिया है मैंने अपने तात्त्विक स्वरूप को ।
३७. मेरा शरीर आनन्द से लबालब भरा हुआ है
तीनों हृदय-ग्रन्थियों का उच्छेदन हो गया है।
समस्त सम्बन्ध समाप्त हो गये हैं।
समस्त बन्धन कट गये हैं।
तीनों अग्नियाँ बुझ गयी हैं।
पंचक्लेश दग्ध हो चुके हैं।
पुराना अज्ञान समाप्त हो गया है।
माया लज्जावश अपना मुँह छिपा रही है।
निर्धनता, अविद्या, रोग समाप्त हो गये हैं।
मैं आनन्द-सागर में तैर रहा हूँ।
मैं प्रकाश, परमानन्द, शान्ति और सामंजस्य से परिपूर्ण हूँ।
मैंने भूमा-परमानन्द का अनुभव कर लिया है।
समस्त अन्धकार नष्ट हो गया है।
समस्त विश्व मुझमें समा गया है।
मैं चिदानन्दघन बन गया हूँ।
मेरा हृदय आनन्द से लबालब भरा हुआ है ।
३८. रोग ! तुम्हारा स्वागत है
रोग ! तुम्हारा स्वागत है।
पीड़ा! तुम्हारा स्वागत है।
रोगाणुओ! तुम्हारा स्वागत है।
मृत्यु ! तुम्हारा स्वागत है।
मलेरिया! पायरिया! हैजा ! टाइफाइड!
तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है।
मुझे तुम सबसे भय नहीं लगता।
तुम मेरा अपना ही प्रकटीकरण तो हो ।
भ्रान्ति का मोतियाबिन्द नष्ट हो चुका है।
अब मुझे सर्वत्र प्रकाश और सत्य के दर्शन हो रहे हैं।
तुम सब मेरे शरीर में मेरे परम प्रिय अतिथि हो।
स्वास्थ्य और रोग आत्मानन्द के सागर की दो लहरें हैं।
पीड़ा भी मेरे लिए सुख ही है।
३९. मैं अब पूर्ण हूँ
मुझे ब्रह्मविद्या का रहस्य ज्ञात है।
मैंने अपने तात्त्विक स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है।
माया मुझसे छिपती फिर रही है।
अपना चेहरा वह मुझे नहीं दिखा सकती।
उसे मेरे सामने आने में संकोच लगता है।
मैं स्वयं सर्वव्यापक अनन्त सत्ता हूँ-
तो अब मैं कहाँ जाऊँ !
मैं स्वयं आप्तकाम हूँ।
समष्टि मेरे अधिकार में है ।
परिपूर्णता के अनुभव के द्वारा
मेरी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो गयी है।
तो अब किस पदार्थ की कामना करूँ !
किस वस्तु को ग्रहण करूँ !
किस वस्तु का त्याग करूँ !
क्या कार्य करूँ अब !
क्या उपलब्ध करूँ अब !
किसे खोजूँ अब !
मैं पूर्ण हो गया हूँ।
मैं प्रज्ञाशील चिद्घन हो गया हूँ।
तो क्या पढूँ अब !
केवल मैं ही मैं हूँ।
तो अब किसके समक्ष भाषण दूँ!
४०. लघु 'मैं' परम दीप्ति से एकाकार हो गया
मैं गंगा तट पर एक शिला-खण्ड पर बैठा था ।
गंगा मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया।
मैंने ॐ – जो ब्रह्म का प्रतीक है-
तथा उसके अर्थ का ध्यान किया।
मेरा लघु व्यक्तित्व विलीन हो गया।
आत्मा की नश्वर सीमा शिथिल पड़ने लगी।
मैं सबसे परे, नाम-रहित लोक में पहुँच गया।
वहाँ था एक अनन्त विस्तार ।
मैंने एकत्व के सर्वोत्कृष्ट परमानन्द का साक्षात्कार किया।
उस पुलक का, प्रसन्नता का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता।
वह पुलक का, प्रसन्नता का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता।
वह एक उदात्त गुह्य अनुभव था-
जिसमें था प्रसन्नता का दिव्य तथा चरम उत्कर्ष ।
यह तेजोमय आनन्द की स्थिति थी ।
मेरा लघु 'मैं' इस स्थिति में व्याप्त उद्दीप्त प्रभा से एकाकार हो गया।
जो दो थे, वे एक हो गये ।
४१. अतिचैतन्यावस्था
मैंने ॐ का जप किया।
ॐ का उच्चारण किया।
ॐ का गान किया।
ॐ का ध्यान किया।
मेरी वैयक्तिकता धीरे-धीरे लुप्त होती गयी।
वह अनन्त सत्ता में विलीन हो गयी।
वैयक्तिकता का लोप किसी प्रकार के समापन का संकेतक नहीं है।
यही तो वास्तविक, पूर्ण तथा शाश्वत जीवन है।
यही भूमा अनुभव है ।
यह उच्च अवस्था सचमुच वर्णनातीत है।
इस अवस्था में सम्भ्रम या भ्रान्ति के लिए कोई स्थान नहीं है।
यह अनिर्वचनीय परमानन्द की अवस्था है।
इसमें है सब कुछ नितान्त स्पष्ट ।
इसमें है सब कुछ हस्तामलकवत् नितान्त निश्चित ।
इस अवस्था में मृत्यु एक असम्भवता है।
इस अवस्था में अनवरत रूप से अमृत प्रवाहित होता रहता है।
प्रज्ञा अपनी गहन दीप्ति से प्रकाशित होती रहती है तथा-
पूर्ण शान्ति का एकछत्र शासन रहता है।
४२. . मैं 'वह' बन गया हूँ
माया से निर्मित संसार अब लुप्त हो गया है।
मनः पूर्णतः नष्ट हो गया है।
परस्पर दूरी उत्पन्न करने वाली अभेद्य सीमारेखाएँ समाप्त हो गयी हैं।
नाम-रूपों का लोप हो गया है।
समस्त विभेद अन्तर नष्ट हो गये हैं।
प्राचीन जीवत्व विलीन हो गया है।
सत्य, प्रज्ञा और परमानन्द की बाढ़ आ गयी है।
एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है।
सर्वत्र अखण्ड समरूप आनन्द-सार व्याप्त हो रहा है।
मैं 'वह' बन गया हूँ।
मैं 'वह' बन गया हूँ।
शिवोऽहम् ! शिवोऽहम् !! शिवोऽहम् !!!
४३. मैंने उसे पा लिया
मैंने उसे यहाँ वहाँ ढूँढ़ा और
अन्ततः मन की शान्ति में
मैंने उसे पा ही लिया ।
वह आश्चर्यों का भी आश्चर्य है।
वह एक ऐसा अमृत है जिससे कभी तृप्ति नहीं मिलती।
ज्ञान की सीमा 'उसी' में समाप्त हो जाती है।
वह महान् आद्य सत्ता है।
वह मधुर स्वर्गीय मधु है
जो जरा और मृत्यु का नाश कर डालता है।
वह अनन्त आदिम प्रकाश है।
वह एक मधुर औषधि है
जो अनश्वरता प्रदान करती है।
मैं उसे 'माधुर्य की राशि' कह कर पुकारता हूँ।
मैं उसे 'परमानन्द का सागर' कह कर पुकारता हूँ।
मैं उसे उपनिषद् का 'पुराण पुरुष' कह कर पुकारता हूँ ।
मैं उसे 'क्षीरसागरशायी' कह कर पुकारता हूँ।
४४. रहस्यात्मक अनुभव
ब्रह्म मधु से भी अधिक मधुर है।
मुरब्बा, मिसरी, रसगुल्ला, लड्डू से भी अधिक मीठा है।
मैंने निर्विकार ब्रह्म का ध्यान किया।
मैं उस स्थिति में पहुँच गया जो ससीमता से परे है।
मेरे अन्दर वास्तविक प्रकाश चमकने लगा।
अविद्या का पूर्णतः नाश हो गया।
इन्द्रिय-कपाट बन्द हो गये ।
इन्द्रियाँ परावर्तित हो गयीं।
श्वास और मन अपने स्रोत में विलीन हो गये।
मैं परम प्रकाश से एकाकार हो गया।
यह एक अकथनीय रहस्यात्मक अनुभव था।
शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम्, सोऽहम्,
सत्, चित्, आनन्द स्वरूपोऽहम् ।
४५. महान् भूमा-अनुभव
मैंने अपने को महान् अनन्त आनन्द में विलीन कर दिया।
मैं अनश्वर परमानन्द के सागर में तैरने लगा।
मैं अनन्त शान्ति के सागर में तैरने लगा।
मेरा अहंभाव विलीन हो गया।
विचारों का आवेग शान्त हो गया।
बुद्धि निष्क्रिय हो गयी।
इन्द्रियाँ आत्मलीन हो गयीं।
संसार का मुझे कोई भान नहीं रहा।
मैंने अपने को प्रत्येक स्थान पर देखा ।
यह एक समरूप अनुभव था ।
उसमें न अन्तर था, न बाह्य था।
न 'यह' था, न 'वह' था;
न 'यहाँ' था, न 'वहाँ' था,
न 'वह' था, न 'तुम' था, न 'मैं' था।
न आकाश था, न काल ।
न विषय था, न पदार्थ ।
न ज्ञाता था, न ज्ञेय था, न ज्ञान था।
न द्रष्टा था, न दृश्य का, न दृष्टि थी।
इस लोकोत्तर अनुभव का वर्णन कोई करे भी तो कैसे करे !
भाषा सीमाओं में बँधी है।
शब्द शक्तिहीन हैं।
स्वयं इस अनुभव का साक्षात्कार करें और स्वतन्त्र हो जायें।
४६. ॐ का गीत
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ ब्रह्म का प्रतीक है।
ॐ परम शक्ति का शब्द है।
ॐ वेदों का प्रणव है।
ॐ समस्त भाषाओं का स्रोत है।
मैं ॐ का गान करता हूँ। मैं ओमोच्चार करता हूँ।
मैं ॐ का ध्यान करता हूँ।
मैं ॐ का जप करता हूँ।
मधुर ॐ का स्वर्गीय संगीत
मेरे हृदय में गूँजता है।
शाश्वत ॐ का दिव्य प्रहर्ष
मुझे प्रेरणा देता है, मेरा उन्नयन करता है
तथा मेरे अन्तरतम में एकत्व का भाव उत्पन्न करता है।
ध्यान के सूत्र
१. मैं शाश्वत जीवन हूँ
सोऽहम् हंसः ।
मैं परम चेतना हूँ।
मैं पूर्ण आह्लाद हूँ।
मैं पूर्ण परमानन्द हूँ ।
मैं पूर्ण ज्ञान हूँ ।
मैं शाश्वत जीवन हूँ ।
मैं अनन्त, शाश्वत और अनश्वर हूँ।
मैं सत्य, प्रज्ञा और प्रकाश हूँ।
२. वेदान्ती ध्यान (क)
मैं आयु-रहित हूँ।
मैं जन्म-रहित हूँ ।
मैं मृत्यु-रहित हूँ।
मैं काल-रहित हूँ ।
मैं दि-रहित हूँ ।
मैं कारण-रहित हूँ।
मैं निर्गुण हूँ।
मैं निराकार हूँ।
मैं निर्भय हूँ ।
मैं निर्विकार हूँ।
मैं अनाम हूँ।
३. मैं ही स्रोत हूँ
मैं समस्त वस्तुओं का स्रोत हूँ ।
मैं अनादि हूँ।
मैं अनन्त हूँ।
मैं प्रत्येक वस्तु का मूल (तत्त्व) हूँ।
मैं सर्वव्यापक हूँ ।
मैं ही शक्ति तथा ऊर्जा का स्रोत हूँ ।
मैं अद्वय, पूर्ण, अन्यून तथा निर्विकार हूँ।
मैं निराकार, निर्विकार तथा अविभाज्य हूँ।
मैं ही नीति, मार्ग तथा जीवन हूँ।
मैं जीवन का स्रोत हूँ ।
मैं प्राण तत्त्व हूँ।
मैं सच्चिदानन्द हूँ ।
४. मैं सर्व हूँ
मैं अमर तत्त्व हूँ।
मैं अनन्तता हूँ।
मेरे ही अन्दर समस्त संसार है।
मैं प्रत्येक प्राणी की आत्मा हूँ।
मैं दिक्काल रहित हूँ ।
मैं अनादि और अनन्त हूँ।
मैं निर्विकार हूँ।
मैं सर्व हूँ।
मैं सर्वस्व हूँ।
मैं एक हूँ, मैं ही अनेक हूँ।
५. मैं सत् हूँ
मैं सर्वस्व हूँ।
मैं सब कुछ हूँ।
मैं प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हूँ।
६. ध्यान - सूत्र
सोऽहम् हंसः ।
मैं सर्वव्यापक जीवन हूँ।
मैं सर्वव्यापक आत्मा हूँ ।
मैं कभी पराजित नहीं होता,
मैं कभी असफल नहीं होता,
मैं कभी हानि नहीं उठाता ;
क्योंकि मैं शाश्वत हूँ
मेरे अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं है।
ब्रह्माण्ड प्रकट हो और लुप्त हो जाये,
सूर्य प्रकट हो और लुप्त हो जाये,
मैं सदैव एक-सा रहता हूँ ।
मैं निरपेक्ष सत्ता
७. वेदान्ती ध्यान (ख)
मैं सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निराकार परब्रह्म हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अद्वैत परब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अखण्ड परिपूर्ण ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं नित्य, शुद्ध, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ (सच्चिदानन्दस्वरूपोऽहम्)------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं भूमानन्दस्वरूप हूँ (भूमानन्दस्वरूपोऽहम् ) -------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं ज्योतिस्वरूप हूँ (ज्योतिः स्वरूपोऽहम् )- --------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं शान्तिस्वरूप हूँ (शान्तिस्वरूपोऽहम् ) ---- ------------------------------------------------ ॐ ॐ ॐ
मैं नित्य-शुद्ध-स्वरूप हूँ (नित्यशुद्धस्वरूपोऽहम्)-- ---------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं नित्य-बोध-स्वरूप हूँ (नित्यबोधस्वरूपोऽहम्)--- -------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं नित्य-मुक्त-स्वरूप हूँ (नित्यमुक्तस्वरूपोऽहम्)-- ------------------------------------------ ॐ ॐ ॐ
मैं नित्य-तृप्ति-स्वरूप हूँ (नित्यतृप्तिस्वरूपोऽहम्) --------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं नित्य-विज्ञान-स्वरूप हूँ (नित्यविज्ञानस्वरूपोऽहम्)------------------------------------------ ॐ ॐ ॐ
मैं नित्य-चैतन्य-स्वरूप हूँ (नित्यचैतन्यस्वरूपोऽहम्)------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं समस्त भूतों की आत्मा हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सर्वस्व हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सबका आधार हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अनुभवातीत हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं जाति*पन्थ-वर्ण से रहित ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं नित्य निष्कल ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निर्मल निष्क्रिय ब्रह्म हूँ ---------------------- ------------------------------ ॐ ॐ ॐ
मैं अखण्ड एकरस चिन्मात्र ब्रह्म हूँ (अखण्डैकरसचिन्मात्रोऽहम् ) ----------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म हूँ (निर्विशेषचिन्मात्रोऽहम्)------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं केवल चिन्मात्र ब्रह्म हूँ (केवलचिन्मात्रोऽहम्)------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं केवल सन्मात्र ब्रह्म हूँ (केवलसन्मात्रोऽहम्)--------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं प्रज्ञानघन ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं विज्ञानघन ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं चिद्घन ब्रह्म हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं आनन्दघन ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं चिन्मय ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं आनन्दमय ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं तेजोमय ब्रह्म हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निराकार, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निरुपाधि निष्कल ब्रह्म हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निर्भय निरवयव ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सचमुच वह ब्रह्म हूँ—जो अद्वैत सूक्ष्मातिसूक्ष्म सब पदार्थों का
प्रकाशक, शाश्वत, शुद्ध तथा अचल है ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सत्यं ज्ञानं-अनन्तं ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अनादि अनन्त ब्रह्म हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अमृत-अविनाशी ब्रह्म हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अधिष्ठान तथा अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं मायातीत ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं द्वन्द्वातीत ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं त्रिगुणातीत ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं भावातीत ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं नाद-बिन्दु-कलातीत ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अव्यक्त- अनुस्यूत ब्रह्म हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं आकाशवत् नित्य ब्रह्म हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं देश-काल-विवर्जित गगन-सदृश निरालम्ब ब्रह्म हूँ .----------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं शान्त, अजर, अमृत, अभय, परब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं दिव्य अमूर्त, अप्राण, अमन ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं शाश्वत, स्वतन्त्र, कूटस्थ ब्रह्म हूँ - --------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं असंग ब्रह्म हूँ (असंगोऽहम् ) ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निरंजन ब्रह्म हूँ (निरंजनोऽहम् ) ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं कूटस्थ ब्रह्म हूँ (कूटस्थोऽहम् ) ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं केवल ब्रह्म हूँ (केवलोऽहम् ) ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं स्रोत हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं परम हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं शिव हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं 'वह' हूँ (सोऽहम्) ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं चैतन्य हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं साक्षी हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं द्रष्टा तथा उपद्रष्टा हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं वेत्ता हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अद्वैत हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अखण्ड चिदाकाश ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अधिष्ठान ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अव्यय अक्षर ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निर्मल ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं विज्ञान-विग्रह ब्रह्म हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अतीन्द्रिय ब्रह्म हूँ (अतीन्द्रियोऽहम् ) ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निरामय ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निरावरण ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अतिसूक्ष्म ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निर्द्वन्द्व ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं नित्य निरूपाधिक निरतिशय आनन्द ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निर्लिप्त ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अशब्द, अरूप और अगन्ध ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निश्चल ब्रह्म हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अवाड्मनोगोचर ब्रह्म हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निर्दोष निर्विकल्प ब्रह्म हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अनिर्देश्य अदृश्य ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं कालातीत, देशातीत ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अमल, विमल, निर्मल ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अचिन्त्य और अव्यवहार्य ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सबमें समान हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं पुरुषोत्तम हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं ईश हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं श्रेष्ठ हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं शिव हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं भाषा-रहित हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निषेध्य-रहित हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मेरे लिए कोई गम्य स्थान नहीं है ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अन्तरतम के भी अन्दर हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं व्यक्त ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अव्यक्त ब्रह्म हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अन्तर्यामी ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अनुभवातीत त्रिगुणातीत अनन्त ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं कारण ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं कार्य ब्रह्म हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सर्व हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सर्वस्व हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सबमें हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
सब मुझमें हैं। ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं ही विविध रूपों में हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
जब रात्रि में सब सो जाते हैं, तब मैं सतत जागता रहता हूँ ------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
जब महाप्रलय होती है, तब भी मैं चमकता रहता हूँ --------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं ही एकमात्र आद्य सत्ता हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं एकाकी हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं ही द्वन्द्व-रहित हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अब आँखों के बिना देखता हूँ। ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अब कानों के बिना सुनता हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अब जिह्वा के बिना स्वाद का अनुभव करता ------------------------------------------------ ॐ ॐ ॐ
मैं अब त्वचा के बिना स्पर्श का अनुभव करता हूँ ----------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अब नासिका के बिना सूघता हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अब पैरों के बिना चलता हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अब हाथों के बिना पकड़ता हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अब मन के बिना जानता हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं विशुद्ध चेतना हैं। ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं प्रत्येक वस्तु का गर्भ हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं इस संसार का मूल हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं प्रत्येक वस्तु का अधिष्ठान हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं परम धाम हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं केन्द्र हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं आधारशिला हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं उद्गम हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मुझमें ही समस्त संसार विघटित होता है ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अगाध ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अप्रमेय ब्रह्म हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अव्यपदेश्य ब्रह्म हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं नेति नेति सिद्धान्त तथा वेदान्त के भाग-त्याग-लक्षण द्वारा निर्दिष्ट
ब्रह्म हूँ। मैं वह ब्रह्म हूँ जो प्राणियों की हृदय गुहा अथवा दहराकाश
में निवास करता है। मैं वह ब्रह्म हैं जिसका साक्षात्कार साधक तप,
ब्रह्मचर्य, सत्य, दम तथा स्वाध्याय के माध्यम से करना चाहते हैं।---------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं पूर्ण हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अनन्त हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निर्विकार तथा अविनाशी हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं प्रज्ञा-रूप हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं नितान्त एकाकी हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अनासक्त हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं कर्म-रहित हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अलिंग हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं पुरातन सत्ता हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं शान्ति का मूर्त रूप हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं हरि हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सदाशिव हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं इन्द्रियों द्वारा अस्पृष्ट हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निराकार तथा अनन्त हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं दिक्काल से परे हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं विश्वाधार हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं सर्वव्यापक हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निरपेक्ष सत्ता हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निरपेक्ष ज्ञान हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं 'वह' हूँ, मैं 'वह' हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं परम सत्ता हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं ही समष्टि हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं मुक्त हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं तटस्थ साक्षी हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
सूक्ष्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अविनाशी हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं निरवयव हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं उद्गम-रहित हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अद्वितीय हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
८. निर्गुण ध्यान (क)
मैं विशुद्ध आत्मा हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
शुद्ध परमानन्द हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अनश्वर हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अनाम तथा अरूप हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं शान्ति तथा परमानन्द का सागर हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अनन्तता हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं प्रकाशों का प्रकाश हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
९. अमूर्त ध्यान
शान्ति का ध्यान करें।
परमानन्द का ध्यान करें।
प्रेम, परमानन्द का ध्यान करें।
भलाई का ध्यान करें।
सत् का ध्यान करें।
चित् का ध्यान करें।
यह अमूर्त ध्यान है।
यह निराकार निर्गुण ध्यान है।
१०. निर्गुण ध्यान (ख)
मैं सत्य हूँ।
मैं अद्वितीय हूँ ।
मैं समस्त वस्तुओं का प्रकाश हूँ।
मैं कूटस्थ हूँ।
मैं शुद्ध चेतना है।
मैं चित् से परिपूर्ण एकमात्र सारतत्त्व हूँ।
मैं वेदान्त का सारतत्त्व हूँ।
मैं चिदाकाश हूँ ।
मैं निष्कलंक तथा निष्पाप हूँ।
मैं मुक्त हूँ, मैं असीम हूँ।
११. सभी आत्माओं में अन्तर्निहित एकत्व का साक्षात्कार करें
मैं विश्व के साथ एकात्म हूँ . ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं ब्रह्म के साथ एकात्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं प्रत्येक प्राणी के साथ एकात्म हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं अमर आत्मा हूँ. ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं असीम तत्त्व के अनुरूप हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
मैं मित्र शत्रु के साथ एक हूँ ---------------------------------------------------- ॐ ॐ ॐ
१२. मैं हूँ
मैं हूँ, मेरी सत्ता है।
मैं सच्चिदानन्द हूँ।
मैं सोचता हूँ; अतः मेरी सत्ता है।
मैं अमर आत्मा हूँ।
मैं सर्वव्यापक अनन्त आत्मा हूँ।
मैं आत्म-सम्राट् हूँ।
मैं आत्मा के राज्य का सम्राट् हूँ।
मैं अद्वैत परमानन्दपूर्ण सारतत्त्व हूँ।
मैं नितान्त मुक्त, पूर्ण तथा स्वतन्त्र हूँ।
मैं विश्व का अधिपति हूँ ।
मैं प्रत्येक प्राणी में निवास करता हूँ।
मैं आत्म-दीप्त, आत्म-स्थित-
आत्मज्ञान तथा आत्मानन्द हूँ।
शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम्, सोऽहम्,
सच्चिदानन्दस्वरूपोऽहम् ।
१३. मैं एक हूँ
मैं एक हूँ ।
मैं ही एकमात्र हूँ।
मैं अद्वितीय हूँ।
मैं अद्वैत हूँ ।
१४. सोऽहम् हंसः
सोऽहम् अस्मि
अहं अस्मि सोऽहम् हंसः मैं हूँ ।
१५. मैं अमृत हूँ
मधुर पीयूष हूँ। मैं
मैं अमरत्व का जल हूँ।
मैं अमृत हूँ।
मैं शाश्वत परमानन्द हूँ।
मैं विशुद्ध आनन्द हूँ।
मैं अनन्त आनन्द हूँ।
मैं शान्ति का सागर हूँ।
मैं प्रसन्नता का स्रोत हूँ।
१६. वेदान्ती ध्यान के लिए सूत्र
अहं आत्मा गुडाकेश।५
अहं आत्मा निराकार सर्वव्यापी स्वभावतः ।
मैं निराकार तथा सर्वव्यापी आत्मा हूँ।"६
अहं ब्रह्म अस्मि (मैं ब्रह्म हूँ) ।
मैं भूमा सदाशिव (मैं अनन्त सदाशिव हूँ) ।
अहं ब्रह्म अस्मि शिवोऽहम् सोऽहम्, सच्चिदान्दस्वरूपोऽहम्,
हंसः सोऽहं, सोऽहं हंसः
(वह मैं ही हूँ, मैं ही वह हूँ, मैं ही वह हूँ, वह ही मैं हूँ)
अहं ब्रह्म अस्मि, ब्रह्मैवाहं अस्मि;
मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में ही हूँ ।
शिवोऽहम्, शिव केवलोऽहम् ;
मैं शिव हूँ, मैं अद्वितीय शिव हूँ।
-------------------------------------------------------------
५ दमश अध्याय, श्रीमद्भगवद्गीता ।
६ अवधूतगीता
१७. वेदान्ती स्वीकरण
मैं अनश्वर, सर्वव्यापी आत्मा हूँ।
मैं निर्विकार, अमर आत्मा हूँ।
मैं सदा से स्वतन्त्र हूँ, स्वतन्त्र हूँ, स्वतन्त्र हूँ ।
मैं सर्वशक्तिमान् तथा सर्वज्ञ हूँ ।
मैं अनन्त, शाश्वत, अविभाज्य ब्रह्म हूँ ।
मैं नितान्त पूर्ण, स्वतःपूर्ण आत्मा हूँ ।
मैं आत्म-दीप्त, आत्म-स्थित पुरुष हूँ ।
मैं सदैव शान्तिपूर्ण, पूर्णतया परमानन्दपूर्ण उच्चतर आत्मा हूँ ।
मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ।
१८. निर्गुण ध्यान के लिए सूत्र
(१)
मैं एकमात्र सूक्ष्म अमर सत्ता हूँ।
मैं तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूँ।
मैं निष्कल तथा अद्वितीय हूँ ।
मैं शुद्ध हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ।
मैं शाश्वत हूँ, आत्मदीप्त हूँ
मैं निष्कलंक हूँ, गतिहीन हूँ, अनन्त हूँ।
मैं अमर हूँ, अजन्मा हूँ, असीम हूँ।
मैं निर्गुण हूँ; तथा अकर्ता हूँ।
मैं शाश्वत रूप से स्वतन्त्र तथा अक्षय हूँ।
मैं अजर तथा अक्षर हूँ।
चिदानन्दरूप शिवोऽहम् शिवोऽहम् ।
मैं चिदानन्दरूप शिव हूँ।
(२)
मैं पूर्णतः बलवान्, समर्थ तथा सुन्दर हूँ।
मैं शाश्वत जीवन हूँ। मैं असीम तथा अनन्त हूँ ।
मैं सदा-सर्वदा स्वतन्त्र हूँ, स्वतन्त्र हूँ, स्वतन्त्र हूँ।
मैं भव्य तथा अलौकिक जीवन हूँ।
मैं पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ।
मैं अनन्त अनश्वर हूँ।
मैं पूर्णतः साहस ही हूँ।
मैं प्रज्ञा, शान्ति और परमानन्द का मूर्त रूप हूँ।
१९. मैं कौन हूँ?
शान्तिपूर्वक बैठें और विचार करें मैं कौन हूँ?
इससे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जायेगा।
इससे स्वतन्त्रता तथा अनश्वरता की प्राप्ति होगी।
इससे पीड़ाओं और दुःखों का नाश होगा।
अस्थि-मांस- युक्त यह शरीर मैं नहीं हूँ।
यह शरीर जड़, नाशवान् तथा सावयव है।
ये इन्द्रियाँ, नेत्र, कर्ण, नासिका मैं नहीं हूँ।
ये तत्त्वों के ससीम उत्पाद हैं।
पंचप्राण मैं नहीं हूँ।
वे रजोगुण से उत्पन्न जड़ उत्पाद हैं।
सन्देह करने वाला मन मैं नहीं हूँ।
यह भी जड़, ससीम तथा नाशवान् है।
मैं हूँ सच्चिदानन्द ब्रह्म
मैं हूँ नित्यमुक्त, शुद्ध, बुद्ध ब्रह्म
मैं हूँ निर्विकार, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्म
मैं हूँ अखण्ड परिपूर्ण व्यापक ब्रह्म ।
तलवार और शस्त्र मुझे काट नहीं सकते।
अग्नि और एटम बम मुझे जला नहीं सकते
जल तथा प्लावन मुझे भिगा नहीं सकते।
बवण्डर तथा वायु मुझे सुखा नहीं सकते।
वेद, बाइबिल, कुरान, अवेस्ता ने मेरा ही गुणगान किया है।
ऋषि-मुनियों ने, योगियों ने मेरा ध्यान किया है।
अभि तथा वायु मेरे आदेशों का पालन करते हैं।
बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा सूर्य मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है।
मैं हूँ अनन्त, शाश्वत, अनश्वर आत्मा ।
मैं हूँ नितान्त परमानन्दपूर्ण, स्वतःपूर्ण आत्मा ।
मैं हूँ सर्वव्यापी आत्मदीप्त पुरुष ।
मैं अजन्मा, अमर, कालातीत ब्रह्म ।
मैं हूँ अप्रभावित, अकर्ता, मूक साक्षी ।
मैं हूँ वेदों का स्रोत, इस संसार की योनि तथा आधार ।
मैं हूँ आन्तरिक शासक, अन्तर्यामी समरूप सार ।
मैं हूं समस्त देवों का देव तथा हिरण्यगर्भ का पूर्वज ।
२०. मैं कितना स्वतन्त्र हूँ
मैं कितना स्वतन्त्र हूँ!
मैं परम स्वतन्त्र हूँ!
मैं हूँ मुक्त जन्म, मरण, क्लेश, दुःख, अज्ञान से।
वह सब, जिसने मुझे संसार में धकेला है।
नष्ट हो गया है।
मैं कितना स्वतन्त्र हूँ!
चिन्ताओं से मैं कितना मुक्त हूँ !
यह भगवत्कृपा है।
अब मैं सब अशुद्धियों से मुक्त हो गया हूँ।
मैं नीरवता के धाम में निवास करता हूँ।
अब कोई मुझे क्षुब्ध या विभ्रान्त नहीं कर सकता।
जीत लिया है सब-कुछ मैंने।
परमानन्द की लहरें मुझे बहाये लिये जा रही हैं।
स्वतन्त्रता की श्वास मुझे उड़ाये लिये जा रही है।
नित्यमुक्तस्वरूपोऽहम्
मैं शाश्वत रूप से स्वच्छन्द रस अथवा सार है।
अब मुझे किसी के आगे घुटने नहीं टेकने हैं।
अब किसी को मात्र प्रसन्न करने के लिए नमस्कार नहीं करना है।
अब किसी की जी हुजूरी नहीं करनी है।
अब चापलूसी करने के लिए किसी का 'आज्ञाकारी सेवक' नहीं बनना है।
तीनों लोकों का सम्राट् हूँ-
आत्म-सम्राट् स्वराट् हूँ।
शुद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् निरंजनोऽहम्,
संसार माया परिवर्जितोऽहम् । विशुद्ध, पूर्णतः प्रबुद्ध, निष्कलंक-
संसार के विकारों से मुक्त हूँ मैं ।
२१. मैं सब-कुछ हूँ
(१)
मैं ही विटामिनों को शक्ति प्रदान करता हूँ ।
मैं ही चाय-काफी का उत्तेजक तत्त्व हूँ।
मैं ही भोज्य पदार्थों का पोषक तत्त्व हूँ।
मैं ही मद्य तथा अफीम का मादक तत्त्व हूँ।
मैं ही स्वर्ण, डालर, नोट तथा धनादेश (चेक) हूँ।
मैं ही स्वर्ग का दिव्यान्न हूँ।
मैं ही रोगरोधी टीकों का सारतत्त्व हूँ।
मैं ही समस्त चिकित्सा पद्धतियों का रोगहर तत्त्व हूँ
मैं ही ऐटम बमों की शक्ति हूँ ।
मैं ही मन्त्रियों तथा अधिनायकों का सामर्थ्य हूँ।
मैं ही अहिंसा तथा सत्य का बल हूँ।
मैं ही सहस्रार चक्र का अमृत हूँ।
मैं ही स्वर, भाषा, ॐ तथा वेद हूँ।
मैं ही सब-कुछ हूँ; मैं ही सर्वस्व हूँ।
(२)
मैं ही सब-कुछ हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ ।
मेरे अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है।
मैं ही विश्वात्मा हूँ।
मैं ही अन्तरात्मा हूँ।
मैं ही सबका ताना-बाना हूँ।
सचमुच केवल मेरा ही अस्तित्व है।
मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ।
मैं अब हूँ; मैं था, मैं सदा-सर्वदा रहूँगा ।
मुझमें न दूरी है और न आकाश ।
मैं सत्ता का सागर हूँ।
यह संसार मेरा एक बुलबुला है।
मुझसे एक बूँद गिरी
और वह विश्व बन गयी।
मेरी दीप्ति
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, व्यास तथा अन्य ऋषियों
के रूप में प्रकाशित होती है।
मेरी तात्त्विक प्रकृति असाधारण तथा आश्चर्यजनक है। -
२२. मैं निर्गुण ब्रह्म हूँ
मैं सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म हूँ ।
मैं निष्प्रपंच ब्रह्म हूँ।
मैं नित्य निष्कल ब्रह्म हूँ ।
मैं अखण्ड परिपूर्ण ब्रह्म हूँ।
मैं सदानन्द ब्रह्म हूँ।
मैं निर्मल, निरंजन ब्रह्म हूँ ।
मैं जाति-पन्थ से परे ब्रह्म हूँ।
मैं अनादि, अनन्त ब्रह्म हूँ।
मैं अभेद ब्रह्म हूँ।
अनामय, अविनाशी ब्रह्म हूँ
मैं 'यह', 'वह', 'मैं', 'तुम', 'वह' के भेदभाव से मुक्त ब्रह्म हूँ।
मैं अमल, असंग, निश्चल ब्रह्म हूँ।
२३. मैं विज्ञानघन ब्रह्म हूँ
मैं अत्यन्त अचल ब्रह्म हूँ।
मैं अत्यन्त शाश्वत ब्रह्म हूँ।
मैं केवल सन्मात्र ब्रह्म हूँ।
मैं केवल चिन्मात्र ब्रह्म हूँ।
मैं केवल नादातीत ब्रह्म हूँ ।
मैं संकल्प-विकल्प-रहित ब्रह्म हूँ ।
मैं अनाम, अरूप ब्रह्म हूँ ।
मैं विज्ञानघन ब्रह्म हूँ।
मैं विलक्षण, सर्व-अधिष्ठान ब्रह्म हूँ ।
मैं अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूँ।
मैं स्वयंज्योति ब्रह्म हूँ।
मैं द्वन्द्व-अहंभाव रहित ब्रह्म हूँ ।
मैं दुःख-शोक-रहित ब्रह्म हूँ।
२४. मैं स्वतन्त्र ब्रह्म हूँ
मैं चैतन्यमात्र ब्रह्म हूँ।
मैं निरामय ब्रह्म हूँ।
मैं निरतिशयानन्द ब्रह्म हूँ।
मैं स्वतन्त्र ब्रह्म हूँ।
मैं स्वयम्भू ब्रह्म हूँ ।
मैं परिच्छिन्न ब्रह्म हूँ।
मैं अव्यय अनन्त ब्रह्म हूँ।
शुद्ध विज्ञानविग्रह ब्रह्म हूँ ।
मैं तत्पदलक्ष्य ब्रह्म हूँ।
मैं त्वंपदलक्ष्य ब्रह्म हूँ ।
मैं निर्भय ब्रह्म हूँ ।
मैं अक्षर ब्रह्म हूँ।
२५. मैं ओंकारस्वरूप हूँ
मैं परब्रह्मस्वरूप हूँ।
जहाँ
न ज्ञान है, न अज्ञान,
न मान है, न अपमान तथा
न आधार है, न आधेय ।
वहाँ मन, शरीर आदि की सीमाएँ नहीं हैं।
मैं शुद्ध चैतन्य हूँ-
जहाँ न बन्धन है, न मुक्ति ।
मैं वह परम तत्त्व हूँ, जिसका ध्यान मन करता है।
मैं ओंकारस्वरूप हूँ।
२६. मैं निरावरण ब्रह्मस्वरूप हूँ
मैं अद्वैत परब्रह्मस्वरूप हूँ
जो मन-वाणी से परे है।
मैं शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ
जहाँ न शुभ है, न अशुभ;
जहाँ न आकाश है, न वायु;
जहाँ न अग्नि है, न जल ।
शुद्ध ब्रह्मस्वरूप हूँ
जहाँ न संकल्प है, न वासनाएँ हैं;
जहाँ न विक्षेप है, न आवरण ।
मैं सत्य-ज्ञान-आनन्द-स्वरूप हूँ
ओ समस्त संसार का साक्षी है।
मैं चिन्मात्रस्वरूप हूँ
जहाँ न इन्द्रियाँ हैं, न मन है और
जहाँ न दृश्य है, न द्रष्टा और न दृष्टि
२७. मैं परब्रह्मस्वरूप हूँ
मैं निर्गुण परब्रह्मस्वरूप हूँ।
मैं वह सारतत्त्व हूँ
जिसका सभी वेदान्ती-धर्मग्रन्थ अनुसन्धान किया करते हैं।
मैं आनन्दघन हूँ।
मैं महामौन का फल हूँ।
मैं वह स्वरूप हूँ जिसमें न द्वित्व है और न द्वन्द्व ।
मैं परब्रह्म हूँ जिसमें न सुख है, न दुःख ।
मैं परम तत्त्व हूँ जहाँ न अन्धकार है, न प्रकाश ।
मैं शुद्ध चेतना हूँ जो हृदयग्रन्थि का उच्छेदन करती है।
२८. मैं सत्य-स्वरूप हूँ
मैं सत्य-स्वरूप हूँ।
मैं शान्त-स्वरूप हूँ ।
मैं शुद्ध-सूक्ष्म-स्वरूप हूँ ।
मैं विज्ञान-स्वरूप हूँ।
मैं निर्विकार-स्वरूप हूँ ।
मैं अखण्ड एकरस-स्वरूप हूँ ।
मैं पूर्ण-स्वरूप हूँ।
मैं निवृत्ति, संन्यास-स्वरूप हूँ ।
मैं प्रज्ञानघन-स्वरूप हूँ।
मैं नित्य चैतन्य-स्वरूप हूँ ।
मैं नित्य तृप्ति-स्वरूप हूँ।
मैं मुक्ति-स्वरूप हूँ ।
मैं शान्ति-स्वरूप हूँ।
मैं सच्चिदानन्द-स्वरूप हूँ।
२९. मैं चैतन्य-स्वरूप हूँ
मैं सत्य हूँ जो एकमात्र जीवन्त विद्यमानता है।
मैं स्वरूप हूँ जो महानतम से भी महान् है।
मैं भेद-रहित एकमात्र एकरस सारतत्त्व हूँ।
मैं अखण्ड एकरस - स्वरूप हूँ।
मैं श्रुतियों की पहुँच से परे परम तत्त्व हूँ।
मैं निश्चल-ब्रह्म-स्वरूप हूँ ।
मैं वह तत्त्व हूँ जो समस्त पदार्थों से परे है।
मैं षड्विकारों से रहित चैतन्य-स्वरूप हूँ।
३०. मैं चिन्मात्र-स्वरूप हूँ
मैं पंचकोशों से रहित ब्रह्म-स्वरूप हूँ ।
मैं परम चेतना हूँ जो अन्तरतम के भी भीतर है।
मैं दिक्काल-कारण से रहित ब्रह्म-स्वरूप हूँ।
मैं चिन्मात्र-स्वरूप हूँ जो प्रज्ञा का सारतत्त्व है।
मैं निर्दोष चेतना से परिपूर्ण चिन्मय - स्वरूप हूँ
जहाँ निषेध नहीं है।
मैंअखण्डाकार-वृत्ति द्वारा प्रकाशित पूर्ण ब्रह्मस्वरूप हूँ ।
मैं पूर्ण कार्य-कारण-रहित शुद्ध चेतना हूँ।
३१. मैं सुखघन-स्वरूप हूँ
मैं ब्रह्म हूँ जो मन का संचालन करता है।
मैं नाम-रूप वाले संसार से रहित परम तत्त्व हूँ।
मैं शाश्वतत्व हूँ,
जहाँ समय की सत्ता नहीं है।
शुद्ध ब्रह्म हूँ
जहाँ न अहंभाव है, न दुर्जेय कामुकता ।
मैं ब्रह्म हूँ,
जो गुणों से परे है तथा
जो सत् तथा असत् से परे है।
मैं सदा सुस्थिर सुखघन-स्वरूप हूँ।
मैं स्वरूप हूँ
जहाँ न आगमन है, न गमन है;
न जाग्रत अवस्था है, न स्वप्नावस्था और
न चलने-फिरने के लिए स्थान है।
वहाँ सदा-सर्वदा के लिए परम शान्ति रहती है।
वह स्वरूप सर्वव्यापक है।
३२. मैं आनन्दघन स्वरूप हूँ
मैं केवल परब्रहा - स्वरूप हैं।
वहाँ न दो हैं, न तीन;
न भाग है, न विभाग तथा
न गणना है, न मापन ।
मैं अखण्ड चिदाकाश आनन्दघन स्वरूप हूँ।
मैं निष्कल निर्द्वन्द्व-स्वरूप हूँ।
मैं निरामय, निष्क्रिय-स्वरूप हूँ ।
मैं निराकार, निरवयव-स्वरूप हूँ।
३३. -रहित ब्रह्म हूँ मैं माया-
मैं माया-रहित ब्रह्म हूँ।
मैं देश-काल-वस्तु-परिच्छेद-रहित ब्रह्म हूँ।
मैं स्वजातीय, विजातीय, स्वगत-भेद-रहित ब्रह्म हूँ।
मैं वासना, संकल्प-रहित ब्रह्म हूँ ।
मैं माया - रहित ब्रह्म हूँ ।
मैं देश-काल-पदार्थ से रहित ब्रह्म हूँ ।
मैं आन्तर, बाह्य तथा लिंग-भेद से रहित ब्रह्म हूँ।
मैं कामना-विचारों से रहित ब्रह्म हूँ ।
३४. मैं निराकार, निर्गुण ब्रह्म हूँ
मैं निराकार, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्म हूँ ।
मैं निरुपाधिक निष्कल ब्रह्म हूँ ।
मैं निर्विकार, निर्विकल्प ब्रह्म हूँ ।
मैं अजर, अमर, अविनाशी ब्रह्म हूँ ।
मैं असंग, अकर्ता, अभोक्ता साक्षी ब्रह्म हूँ ।
मैं निरवयव, निर्लिप्त ब्रह्म हूँ ।
मैं अखण्ड, परिपूर्ण ब्रह्म हैं।
मैं निराकार, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्म हूँ ।
मैं निष्कल ब्रह्म हूँ।
मैं निर्विकार तथा अचिन्त्य ब्रह्म हूँ ।
मैं अविनाशी नित्य ब्रह्म हूँ।
मैं अनासक्त, अकर्ता, अभोक्ता ब्रह्म हूँ।
मैं निरवयव तथा अनासक्त ब्रह्म हूँ ।
मैं अविभाज्य तथा सम्पूर्ण ब्रह्म हूँ।
३५. मैं त्रिगुणातीत ब्रह्म हूँ
मैं त्रिगुणातीत ब्रह्म हूँ।
मैं द्वन्द्वातीत ब्रह्म हूँ।
मैं नाद-बिन्दु-कलातीत ब्रह्म हूँ ।
मैं भावातीत ब्रह्म हूँ।
मैं कालातीत ब्रह्म
मैं मायातीत ब्रह्म हूँ।
ध्यानयोग - सूत्र
१. धारणा
१. बाह्य पदार्थ, आन्तरिक बिन्दु या किसी विचार-बिन्दु पर मन को केन्द्रित करना धारणा है।
२. मन को केन्द्रित करना धारणा है। किसी एक विचार के अनवरत प्रवाह को ध्यान कहते हैं।
३. शान्त हो जायें। प्रसन्न रहें। धैर्य रखें। नियमित अभ्यास करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपनी कामनाओं तथा कार्य-कलापों में कमी कर दें। दूसरों के साथ मेल-जोल कम रखें। मौन रखें। ये धारणा के सहायक साधन हैं।
४. त्रिकूट या हृदय पर धारणा का अभ्यास करें।
२. ध्यान (क)
१. जब आप धारणा, ध्यान तथा समाधि का अभ्यास एक-साथ तथा एक ही समय में करते हैं, तब इसे संयम कहते हैं।
२. ध्यान मोक्ष का द्वार खोलता है।
३. ध्यान से प्रातिभज्ञान और शाश्वत परमानन्द की प्राप्ति होती है।
४. ज्वलन्त वैराग्य तथा ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए तीव्र आकांक्षा का पोषण करें।
५. सिद्धियाँ योग-पथ की बाधाएँ हैं। उनसे बच कर रहें।
६. अत्यधिक निद्रा, ब्रह्मचर्य का अभाव, आलस्य, वासनाओं का उद्भव सांसारिक प्राणियों की संगति, अत्यधिक परिश्रम, अति-भोजन- ये ध्यान बाधाएँ हैं। की
७. भगवान् के रूप पर ध्यान करें। यह मूर्त ध्यान है।
८. भगवान् के गुणों का ध्यान करें। यह अमूर्त ध्यान है।
३. ध्यान (ख)
१. धारणा यथासमय ध्यान और समाधि के रूप में विकसित होती है।
२. ध्यान दीर्घ काल तक किया गया धारणा का अभ्यास है। ध्यान की प्रक्रिया अखण्ड तैलधारावत् होती है।
३. प्रारम्भ में ध्यान में अभ्यास का तत्त्व निहित रहता है। बाद में ध्यान एक आदत बन जाता है तथा परमानन्द, प्रसन्नता और शान्ति प्रदान करता है।
४. यम, नियम आदि की प्रारम्भिक अवस्थाओं का अभ्यास करने के बाद ही ध्यान का पूरा लाभ प्राप्त होता है।
५. एकाग्र मन में एक से अधिक विचारों के लिए स्थान नहीं रहता। मन में रहने वाला कोई विचार दूसरे विचार के प्रवेश करने पर ही हटता है।
६. आप चाहे जितने बुद्धिवादी हों, प्रारम्भ में मूर्ति या प्रतीक की सहायता लिये बिना आप मन को एकाग्र नहीं कर सकते।
७. ध्यान में वे साधक शीघ्र सफल हो जाते हैं जिनका अभ्यास गहन होता है।
८. ध्यान एक रचनात्मक, जीवन्त तथा सक्रिय प्रक्रिया है। यह मानवता को देवत्व में रूपान्तरित कर देती है।
९. नियमित ध्यान करके आप अपने चारों ओर एक अपराजेय अभेद्य किला निर्मित कर सकते हैं। तब माया आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती।
१०. ध्यान प्रातिभज्ञान की कुंजी है।
११. नाम-रूपों में आवृत दिव्यता को प्रकट करने की कुंजी ध्यान है।
१२. आध्यात्मिक प्रबोधन की कुंजी ध्यान है।
१३. जीवन-तोष के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ध्यान एकमात्र पारपत्र (पासपोर्ट) है।
१४. ध्यान मृत्यु का प्रतिकारक है।
१५. ध्यान दैनिक जीवन का एक आवश्यक अंग है; अतः प्रतिदिन ध्यान अवश्य करें।
१६. प्रतिदिन किया गया अल्प ध्यान भी आपको किंचित् ऊपर उठा कर भगवान् के थोड़ा निकट ले जायेगा ।
१७. भक्ति तथा ध्यान से मन का परिष्कार होता है।
१८. मूषा (स्वर्ण गलाने का पात्र) में शोधित किया गया स्वर्ण चमकने लगता है इसी प्रकार आत्मा पर किये गये ध्यान से मन शुद्ध तथा अध्यात्म-आभा से देदीप्यमान जाता है।
१९. परिशोधित मन सब कुछ समझ सकता है। यह सूक्ष्मतम विषय, यहाँ तक कि गूढ़ विषयों को भी समझ लेता है।
२०. ध्यान से अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। आत्मा का अनवरत ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
२१. शुचिता तथा इससे सम्बद्ध अन्य गुणों यथा सरलता, निष्कपटता, स्पष्टता, सत्यवादिता, उदारमति, निर्दोषता, अच्छाई का ध्यान करें।
२२. मन को शान्त करके, विचारों और मनोभावों को भी शान्त करके असीम तत्व के साथ संस्वरित हों।
२३. मन एक बहुत बड़ा रेडियो है। इसे असीम तत्त्व के साथ संस्वरित करें। परमात्मा के परमानन्द का रस लें।
२४. ध्यान करें। दिव्यता में अपने को सुस्थिर करें।
२५. ध्यानावस्था में चेतन मन – जो बाह्य संसार, शरीर और इसकी आवश्यकताओं के बारे में सोचा करता है—के द्वार बन्द कर दें।
२६. ब्रह्म का ध्यान धर्म का सर्वोच्च स्वरूप है।
२७. जब मन शान्त और अविक्षुब्ध होगा, तभी ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकेगा।
२८. हे राम! ब्राह्ममुहूर्त में नियमित रूप से ध्यान करें और अपने मन को आत्मानन्द का स्वाद लेने दें।
२९. ध्यान करने की मनःस्थिति आती-जाती रहती है। इन्द्रियों का निग्रह करें। सदैव सतर्क रहें।
३०. नियमित रूप से ध्यान करें तथा पहले से अधिक रचनात्मक बन जायें।
३१. निश्चित समय (ब्राह्ममुहूर्त, दोपहर, सायंकाल- झुटपुटा, सान्ध्य-प्र तथा रात्रि) पर ध्यान करने के लिए बैठें।
३२. आपका जीवन ध्यान के साथ एकाकार हो जाना चाहिए।
३३. गहन ध्यान की अवस्था में प्रथम बार हृदय में परमानन्द के साथ दिव्य पुलक का अनुभव होता है।
३४. जब आप गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब आपको सन्तुलन, आत्म-संयम, प्रशान्ति, मानसिक शान्ति, स्थिरता, निर्भयता तथा सर्वोच्च विरक्ति का अनुभव होता है।
३५. आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति, पूर्ण शान्ति, ज्ञान तथा परमानन्द —ये हैं ध्यान के फल ।
३६. नियमित रूप से ध्यान करें। आप ब्रह्म-साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
३७. ध्यान करें। परम तत्त्व की एक झलक का दर्शन करें। समस्त द्वित्व, दुःख तथा क्लेश पूर्णतः नष्ट हो जायेंगे।
४. विचार तथा ध्यान
१. ब्रह्म जिज्ञासा करने से मानव का परम कल्याण होता है। केवल ब्रह्म की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। आप ब्रह्म जिज्ञासा अवश्य करें तत्त्वमसि ।
२. बिना विचार के ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। विचार के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया जाता है— मैं कौन हैं? बन्धन क्या है? संसार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? मोक्ष क्या है?
३. स्वास्थ्य के दुर्ग पर रोग के शत्रु आक्रमण कर देते हैं। ध्यान और ब्रह्म-विचार की तलवार से इन शत्रुओं का नाश कर दें।
४. हे अमृतपुत्र! उत्तिष्ठ! घोषणा करें—मैं अविनाशी आत्मा हूँ। शाश्वत जीवन का अमृत बहा जा रहा है। शीघ्रता करें। नेत्र बन्द करके ध्यान करें और स्वच्छन्दता से अमृत पान करें।
५. जब तक मन पूर्णतः परावर्तित हो कर ब्रह्म में विलीन न हो जाये (भले ही, एक-दो मिनट के लिए), तब तक आसन छोड़ कर उठें नहीं।
६. आपको अधिक शक्ति की आवश्यकता है। आपको यह शक्ति अपने अन्दर से इस विचार का ध्यान करने से प्राप्त होगी मैं आत्मा हूँ। मैं सर्वव्यापी, अविनाशी आत्मा हूँ।
७. आप अपने को कहाँ पाते हैं? क्या आपने अध्यात्म मार्ग पर पहले की अपेक्षा कुछ अधिक उन्नति की है? क्या आप वहीं हैं, जहाँ आप पहले थे? क्या आप पीछे हट रहे हैं? इन बातों का पता लगाने तथा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तुरन्त ही उपयुक्त उपाय काम में लायें। जल्दी करें सतर्क रहें।
८. केवल सांसारिक विचार ही जन्म-मरण के चक्रों को निर्मित करते हैं। अपने विचारों को शुद्ध बनायें । उदात्त दिव्य विचारों को ही मन में प्रवेश करने दें। मन में केवल इसी विचार को स्थान दें-मैं अमर सर्वव्यापक आत्मा हूँ ।
९. अपने विचारों के साक्षी बनें। उनके साथ तादात्म्य स्थापित करें। वे तुरन्त ही मन से निकल जायेंगे। मन दो भागों में विभक्त हो जायेगा एक भाग साक्षी बन जायेगा—यह केवल देखेगा। यह शान्त तथा अविक्षुब्ध रहेगा। मन का दूसरा भाग बनेगा प्रेक्ष्य पदार्थ या अध्ययन का विषय
१०. यदि आपने आत्म-विश्लेषण या आत्म-निरीक्षण करना नहीं सीखा है, तो आप आध्यात्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते।
११. ध्यान का अन्तिम फल मोक्ष है। यह आत्मा की स्वाभाविक तथा शाश्वत स्थिति है। इसका (मोक्ष का) न आदि है और न अन्त।
१२. अनवरत रूप से मन को अनुशासित करते हुए ध्यानाभ्यास के द्वारा आपको अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयत्न करना ही होगा। आध्यात्मिक प्रबोधन द्वारा आप जन्म-मरण के नीरस चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
१३. ब्रह्मज्ञान के स्तर से नीची कोई भी वस्तु आपको आनन्द प्रदान नहीं कर सकती; अतः अपनी अन्तरात्मा का सतत ध्यान करने का प्रयास करें।
१४. अहर्निश इसे दोहरायें-मैं सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ। मैं सदा सर्वदा शुद्ध, सर्वशक्तिमान् तथा सर्वव्यापक हूँ। विचारों का बहुत महत्त्व होता है। जैसा आप विचार करते हैं, वैसा ही आप बनते हैं।
१५. मौन हो जायें और ईश्वर की फुसफुसाहटें सुनें। मौन में कितनी शक्ति होती है? सुमधुर वाणी की अपेक्षा मौन अधिक भावपूर्ण होता है। ध्यान करें तथा मौन का आनन्द लें। मौन! तुम्हारा स्वागत है। तुम शान्ति के अग्रदूत हो। तुम स्वयं शान्ति हो हो ! तुम ब्रह्म हो ! मौन, तुम्हें नमस्कार है।
परम तत्त्व के साथ सम्पर्क करने की प्रक्रिया
१६. आध्यात्मिक परमानन्द के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ध्यान एक सोपान है; अतः शुद्ध हृदय से नियमित ध्यान करें।
१७. मन की एक ऐसी स्थिति होती है जो बाह्य पदार्थों से बिलकुल अप्रभावित रहती है। यह मन की तटस्थ तथा स्वाभाविक स्थिति कहलाती है। ध्यान इसी स्थिति का नाम है।
१८. अपने प्रातिभज्ञान के अतिरिक्त सत्य को जानने का अन्य कोई साधन नहीं है। ‘मैं कौन हूँ' का विचार तथा ध्यानाभ्यास करने से प्रातिभज्ञान के द्वार खुलते हैं।
१९. छिपे हुए खजाने को प्राप्त करने का उपाय खोदने के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है; इसी प्रकार परमानन्द को प्राप्त करने का उपाय ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है।
२०. ध्यान की प्रक्रिया से साधक अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है। मन को ईश्वर पर संकेन्द्रित करना तथा अन्य सभी पदार्थों का बहिष्कार करते हुए केवल ईश्वर का ही विचार करना ध्यान है।
२१. ध्यान के अन्तर्गत वे सभी आध्यात्मिक अभ्यास होते हैं जिनसे मन ब्रह्म पर निश्चित रूप से संकेन्द्रित हो जाता है।
२२. ध्यान मन को संस्वरित तथा सामंजस्यपूर्ण रखता है। ध्यान मन को असीम तत्त्व से संस्वरित रखता है।
२३. ध्यान की प्रारम्भिक अवस्थाओं में ध्याता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ध्याता की रुचि समाप्त होने लगती है तथा वह अपनी साधना रोक देता है। यह एक भयानक त्रुटि है। मित्रवर! परिश्रम करते रहें। वरिष्ठ साधकों की संगति में रहें। अब अपने गुरु के साथ रहें।
२४. ध्यानाभ्यास को आपकी आदत का अंग बन जाना चाहिए। सतत अभ्यास से ही ऐसा हो सकता है—अन्य किसी उपाय से नहीं।
२५. यदि आप शुद्ध हृदय से आत्मा का सतत ध्यान करें, तो अभी ही आपको मोक्ष या परमानन्द की प्राप्ति हो सकती है।
२६. एकान्तवास, संयम (तप), आत्म-नियन्त्रण, धैर्य, अनसूया तथा मिताहार ध्यान के सहायक साधन हैं।
ध्याता और ध्येय मिल कर एक हो जाते हैं
२७. एक ही विचार बिन्दु की सचेतन मानसिक पुनरावृत्ति ध्यान है। जब साधक की यह प्रक्रिया पूर्ण बन जाती है, तब वह उस समाधि-अवस्था में प्रवेश करता है, जिसमें ध्याता और ध्येय मिल कर एक हो जाते हैं।
२८. पिपासु साधक सदैव सतर्क रहता है। अहर्निश उसके विचार शाश्वत ब्रह्म पर ही केन्द्रित रहते हैं। ध्यान से उसे सदैव आनन्द प्राप्त होता रहता है।
२९. ध्यान से आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में निर्मुक्त होती है। यह ऊर्जा सभी असत् विचारों का नाश करके काम-ऊर्जा का उदात्तीकरण कर देती है।
३०. ब्राह्ममुहूर्त में ध्यान के माध्यम से ज्ञान-गंगा में अवगाहन करें। सन्तत्व के परिधान पहनें। सन्तोष के शीतल पेय का सेवन करें।
३१. जिस प्रकार गंगा नदी सागर की ओर प्रवाहित होती है, सागर की ही और ढालू होती है तथा सागर की ही ओर प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करने वाले योगी की जीवन-सरिता समाधि की ही ओर प्रवाहित होती है, समाधि की ही ओर ढालू होती है तथा समाधि की ही ओर प्रवृत्त रहती है।
३२. यदि साधक लम्बे समय तक नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करे, तो निश्चित ही उसकी चेतना का स्तर उच्चतर हो जायेगा। यदि ऐसा न हो, तो उसकी साधना त्रुटिपूर्ण है। सम्भव है, वह ध्यान ही न करता हो। सम्भव है, वह तन्द्रा की स्थिति में हवाई महल बनाता हो।
३३. ब्राह्ममुहूर्त में नियमित रूप से ध्यान करके अमरता का शक्तिवर्धक अमृत पियें। आधा घण्टे तक कीर्तन करके इस अमृत पेय में उदारतापूर्वक परमानन्द - शान्ति को भी मिश्रित कर लें। और
३४. मन को कहीं भी चैन नहीं है। कामनाओं को कभी अन्तिम रूप से सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता। कामना की अग्नि आपके हृदय में धधकती रहती है। ध्यान से प्राप्त आत्मा के अमृत से इस अग्नि का शमन करें।
३५. कभी-कभी ध्यान के अभ्यासी में दम्भ की भावना अंकुरित होने लगती है। वह अपनी साधना में बहक भी जाता है। उसे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा।
३६. परम सत्ता के एकत्व का ध्यान करने से मन अविक्षुब्ध तथा शान्त हो जाता है।
३७. यदि आप निर्गुण, निराकार ब्रह्म के ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब भी आप अपने इष्टदेवता या सगुण ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। निर्गुण ध्यान में सफल होने के लिए आपको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म एक ही हैं।
३८. जन्म-मृत्यु तथा अन्य क्लेशों का कारण है अज्ञान । ब्रह्मज्ञान से अज्ञान समाप्त हो जाता है। अतः ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करें।
३९. आत्म-लाभ से बढ़ कर अन्य कोई लाभ नहीं है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा की पूजा करें। आत्मा का ध्यान निरन्तर करें।
४०. मौन से साधक को शक्ति तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। मौन साधक को पुनरुज्जीवित करता है। अतः मौन में प्रवेश करें। मीन में विलीन हो जायें मौन ब्रह्म है।
५. ध्यान (ग)
१. ब्रह्म के एकमात्र विचार का अविरत प्रवाह ध्यान है।
२. चिरस्थायी शान्ति तथा अमर परमानन्द की ओर ले जाने वाला श्रेष्ठ मार्ग ध्यान है।
३. ध्यान प्रातिभज्ञान की कुंजी है।
ध्यान की पूर्वापेक्षाएँ
४. यदि मन में कामनाएँ हैं और बाह्य पदार्थों द्वारा वह विचलित हो जाता है, तब ध्यान का अभ्यास नहीं किया जा सकता ।
५. यदि आपका मन उच्छृंखल और अनियन्त्रित है; हृदय में दुर्भाव तथा विक्षोभ हैं, तब आप गहन ध्यान नहीं कर सकते।
६. जिस साधक ने यम, नियम तथा प्रत्याहार का अभ्यास कर लिया है, उसे ध्यान का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है।
७. अनुशासन तथा निष्ठा के बिना ध्यान में सफलता नहीं मिलती।
८. धारणा ध्यान की पूर्व-स्थिति है।
साधना में निश्चित सफलता प्राप्त करने हेतु उपयोगी बातें
९. जब सत्त्व की प्रधानता होती है, तब मन शान्त तथा अविक्षुब्ध होता है; तब ध्यान शान्त और स्थिर बन जाता है।
१०. गहन आस्था तथा अतीव रुचि के साथ ध्यान करें। नियमित ध्यान से आपको आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने का उत्साह मिलेगा।
११. जब आप ध्यान के लिए बैठें, तब एक संकल्प करें कोई भी विचार मुझे विचलित नहीं कर सकता। सत्य का साक्षात्कार किये बिना मैं उदूंगा नहीं।' इस प्रकार का निश्चय तथा उपलब्धि में इस प्रकार की प्रतीति ही आपको अपने लक्ष्य के निकट ले जायेगी।
१२. ब्रह्म के स्वभाव तथा गुणों (यथा सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता आदि) का ध्यान करें।
१३. अनन्त, निर्भय, कालातीत, दिग्-रहित, अजन्मा, अनश्वर, अजर, परम आत्मदीप्त ब्रह्म का ध्यान करें।
१४. नियमित रूप से ध्यान करें।
१५. निश्चित समय पर ध्यान करें।
१६. ध्यान को अपनी दिनचर्या का एक अंग बना लें ।
ध्यान में होने वाले अभीप्सित अनुभव
१७. गहन ध्यान की अवस्था में दिव्य पुलक, प्रसन्नता तथा परमानन्द का अनुभव होता है।
१८. गहन ध्यान में आप अपनी अन्तरात्मा के साथ विलीन हो जाते हैं तथा दिव्य अनुभव के आन्तरिक मर्म की गहराइयों तक पहुँच जाते हैं। अहंभाव समाप्त हो जाता है। मन क्रियाशील नहीं रह जाता।
१९. ध्यान में मन एक ही वस्तु या आदर्श में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। उसके ऊपर अन्य किसी वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता। मन की इस तल्लीनता के ही कारण इन्द्रियों के कार्यों का पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाता है।
२०. ध्यान का अगला चरण समाधि है।
ध्यान के परिणाम
२१. पूर्ण शान्ति, ज्ञान, प्रशान्ति, स्थिरता, निर्भयता, विरक्ति, अन्तर्दृष्टि, प्रलोभन—ये हैं ध्यान के सद्परिणाम ।
२२. ध्यान पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करता है।
२३. ध्यान मानव को दिव्यता में रूपान्तरित कर देता है।
२४. ध्यान से सन्देह समाप्त हो जाते हैं।
महत्त्वपूर्ण मर्म
२४. ध्यान मोक्ष का द्वार खोल देता है।
२६. शुद्ध हृदय में ही ध्यान प्रवाहित होता है।
६. ध्यान की प्रक्रिया
ध्यान-विधि
१. ध्यान की प्रक्रिया में आध्यात्मिक अपरोक्ष अनुभव प्राप्त होता है।
२. मौन ध्यान करें। आध्यात्मिक विकास तथा आत्म-साक्षात्कार करें।
३. सुखासन में मेरुदण्ड सीधा करके बैठें। ॐ के अर्थ का ध्यान करते हुए इसका जप करें। मन को विक्षेप उत्पन्न करने वाले विचारों और कामनाओं से मुक्त रखें।
४. यदि आपका ध्यान अपूर्ण है, तो अपने हृदय पर ध्यान दें। सम्भव है, उसमें वासना, राग और अहंभाव की अन्तर्धाराएँ अब भी प्रवाहित हो रही हों; इन्द्रियाँ अब भी उपद्रव मचा रही हों; विषय-सुख की कामनाएं अब भी विद्यमान हों।
५. ध्यानाभ्यास ज्ञान-प्राप्ति का महान् वैज्ञानिक उपाय है।
ध्यान का महत्त्व
६. ध्यान के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। योगी अपनी आत्मा का मन्थन करके सत्य को प्रकट करता है।
७. ध्यान धार्मिक जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष है। सम्यक् ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन को ध्येय में रूपान्तरित होने के लिए अग्रसारित करती है।
८. ब्रह्म-ध्यान अमरता प्रदान करता है। अमर होने का अन्य कोई उपाय नहीं है।
ध्यान का लक्ष्य
९. ध्यान का उद्देश्य प्रातिभज्ञान की सहायता से अनुभवातीत चेतना का साक्षात्कार करना है।
१०. जो ध्यान पथ का अनुसरण करता है, उसे ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा के एकत्व का तथा आत्मा की दिव्यता का ज्ञान होता है।
१९. ध्यान आपको अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा सत्य के निकटतर लाता है।
१२. ध्यान के बाद ही आप समाधि की सर्वोच्च अवस्था में प्रवेश करते हैं।
१३. प्रातिभज्ञान के क्रम विकास के माध्यम से जब आप गुणों से परे हो जाते हैं, तब ध्यान समाप्त हो जाता है।
१४. परम लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात् योगी ध्यान नहीं करता। उसके लिए ध्येय की सत्ता समाप्त हो जाती है; क्योंकि वह कण-कण में सर्वव्यापी ईश्वर के दर्शन करता है।
ध्यान के लाभ
१५. किंचित् ध्यान भी आपको मृत्यु के भय से मुक्त करता है।
१६. ध्यान के सतत अभ्यास से आन्तरिक शान्ति प्राप्त होती है।
१७. ध्यान से मन प्रभावकारी तथा सात्त्विक विचारों एवं प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है।
१८. साकार ईश्वर का दीर्घकालीन ध्यान करने से भक्त के हृदय में इष्टदेव के प्रति गहन प्रेम की भावना उत्पन्न होती है।
१९. ध्यानावस्था में आपको सीधे ही ईश्वर से भरपूर सत्त्वगुण प्राप्त होता है।
२०. जो साधक नियमित रूप से ध्यान करता है, उसे शक्ति, प्रसन्नता तथा स्वतन्त्रता प्राप्त होती है।
२१. ध्यान एक शक्तिवर्धक तथा पुनरुज्जीवन प्रदान करने वाली औषधि है। ब्राह्ममुहूर्त तथा सान्ध्य-प्रकाश की शान्त वेला में गम्भीर ध्यान का अभ्यास करें।
२२. ध्यानाभ्यास से निम्न स्तर की समस्त कामनाएँ तथा व्यक्तिगत विचार समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने की एकमात्र कामना बची रहती है।
ध्यान में बाधाएँ
२३. भूतकाल का चिन्तन तथा भविष्य की चिन्ता ध्यान की बाधाएँ हैं।
२४. ध्यान की सबसे बड़ी बाधा स्मृति है।
२५. अतीन्द्रिय अनुभवों की उपेक्षा करें। सतर्क रहें तथा मन को ध्येय पर केन्द्रित करें।
२६. ध्यान गहन, नियमित, गम्भीर तथा अनवरत होना चाहिए।
२७. वैराग्य और ध्यान के द्वारा इन्द्रियों का प्रभाव कम होने लगता है तथा मन परम तत्त्व में विलीन हो जाता है।
२८. मिताहारी बनें। एकान्त-वास करें। ध्यान करें। क्रोध न करें। घमण्ड न करें।
२९. यम, नियम, आसन और प्राणायाम ध्यान की प्रारम्भिक तैयारियाँ हैं।
ध्यान में मन
३०. ध्यान में मन अन्तर्मुखी हो जाता है तथा समस्त विचार तरंगों को रोक देता है।
३१. जैसे ही आप ध्यान के लिए मन का निरोध करते हैं, संस्कार तथा भूतकाल की अनुभूतियाँ ध्यान में विक्षोभ उत्पन्न करने लगती हैं।
३२. जब सत्त्व तथा ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो जाता है तब
आप देवता, आत्मा जैसी सूक्ष्म सत्ताओं के दर्शन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं।
३३. जब आप ध्यान द्वारा प्रातिभज्ञान का विकास करते हैं, तब आत्म-साक्षात्कार होता है।
ध्यान द्वारा आत्म-साक्षात्कार
३४. अपनी अन्तरात्मा का ध्यान करें। तब मन ब्रह्म में लीन हो जायेगा। आप आत्म-साक्षात्कार कर लेंगे।
३५. अहंभाव (जो असत्य पर आधारित आपकी निजता है) को नष्ट करें। स्थिर और शान्त बैठे। ध्यान करें तथा आत्मा का साक्षात्कार करें।
३६. जब आप ध्यान में यथेष्ट सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तब ध्यान-प्रक्रिया के प्रति आपकी सजगता समाप्त हो जायेगी। आप अपने प्रति भी सजग नहीं रह जाते। केवल ध्येय ही शेष रहता है। केवल शुद्ध चेतना की सजगता शेष बचती है।
३७. प्रातिभज्ञान ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान को ब्रह्म में विलीन कर देता है।
३८. आत्मा के ध्यान में शाश्वत शान्ति तथा चिरस्थायी परमानन्द प्राप्त करना सीखें।
३९. जो नियमित ध्यान का अभ्यास करता है तथा समाधि-अवस्था में प्रवेश करता है, उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह दूसरों के लिए वर्तमान इस मायिक संसार से मुक्त हो कर जीवन्मुक्ति की परम अवस्था में पहुँच जाता है।
४०. नीरवता में नियमित रूप से ध्यान करें। आपको प्रेरणा, शान्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति होगी। आपको ईश्वर की महिमा, सत्य के वैभव तथा उसकी सर्वव्यापिता का अनुभव होगा।
७. समाधि
१. समाधि पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था है। यह परम तत्त्व के साथ ऐक्य की अवस्था है।
२. समाधि में सीमाएँ नहीं हुआ करतीं। ज्ञाता तथा ज्ञेय की भी सत्ता नहीं होती। यह एक समरूप (एकरस ) अनुभव है।
३. समाधि की अवस्था में मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है। व्यक्तिकता भी विलीन हो जाती है। चिरस्थायी परमानन्द की प्राप्ति होती है। योगी पीड़ा, दुःख, भव तथा भ्रान्तियों से मुक्त हो जाता है।
४. समाधि में पूर्णतः एकता रहती है। समाधि केवल आत्मा ही है।
५. समाधि परम चेतना की अवस्था है। समाधि में मन की खोज समाप्त हो जाती है; मन विश्राम की उस स्थिति में रहता है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय मिल कर एक हो जाते हैं।
६. मन की वृत्तियों को समाप्त करके आप समाधि की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं।
७. परम तत्त्व (आत्मा) का प्रत्यक्ष ज्ञान ही समाधि है। समाधि परम चेतना है।
८. सफल तथा गहन ध्यान के बाद समाधि की अवस्था में प्रवेश किया जाता है। ९. समाधि व्यक्तित्व का समापन नहीं है, यह उसकी पूर्णता है।
१०. पूर्णत्व का अनुभव समाधि है। क्लेशों से मुक्ति ही समाधि है। समाधि है। परमानन्द ।
११. समाधि की अवस्था में प्राण में गति नहीं होती। तब साधक न श्वास लेता है, न छोड़ता है।
१२. समाधि की अवस्था में न जन्म है, न मृत्यु है; न क्षय है, न रोग तथा न पीड़ा है, न दुःख ।
१३. गहन ध्यान की अवस्था में नाम रूप नहीं रह जाते। तब केवल अनन्त आकाश (Space) की जागरूकता रहती है। बाद में अनन्त आकाश भी लुप्त हो जाता है तथा अनस्तित्व की स्थिति आ जाती है। अकस्मात् ज्ञान अथवा निर्विकल्प समाधि का उदय होता है।
१४. निर्विकल्प-समाधि सर्वोच्च मूल्य का साक्षात्कार है।
१५. निर्विकल्प समाधि में परम तत्त्व का उसकी समग्रता में अन्तर्ज्ञान होता है। यह परम तत्त्व के साथ ऐक्यता का अनुभव है।
१६. समाधि में प्रबोधन प्राप्त होता है। तब निश्चेष्ट जीव-चेतना के स्थान पर ब्रह्म की परम चेतना होती है।
१७. निर्विकल्प समाधि में कोई पदार्थ नहीं होता। समस्त मानसिक वृत्तियों का अवसान हो जाता है।
१८. योगी अपने आध्यात्मिक अनुभव की सर्वोच्च अवस्था - निर्विकल्प - समाधि में ही परम सत्ता का साक्षात्कार करता है।
१९. जब राजयोगी कैवल्य प्राप्त करता है, तब गुण अपने-अपने उद्गम — प्रकृति या प्रधान — की ओर लौट जाते हैं।
२०. बुद्धि, अहंकार, मन तथा इन्द्रियाँ ये तीनों गुणों के मात्र परिणाम हैं। ये (बुद्धि, अहंकार, मन आदि) भी एक-एक करके अपने-अपने मूल स्रोतों में विलीन हो जाते हैं।
२१. केवल पुरुष ही द्रष्टा है। गुण तथा उनके विकार ही दृश्य हैं।
२२. कैवल्य की अवस्था में चित्त, अहंकार तथा बुद्धि मुक्त हो जाते हैं।
२३. कैवल्य की अवस्था में पुरुष अपनी मुक्तावस्था में अवस्थित हो जाता है।
२४. जब पुरुष को कैवल्य प्राप्त हो जाता है, तब गुण तथा उनके परिणामों के पास पुरुष के लिए कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए नहीं रह जाता।
२५. ‘न हम, न तुम, दफ्तर गुम’– मैं, न तुम; मुक्त पुरुष के लिए अब प्रकृति का दफ्तर बन्द हो गया है।
२६. ध्यान और समाधि के परमानन्द के समक्ष विषय-सुख कुछ भी नहीं है।
२७. सहज समाधि में सोऽहं भावना स्वतःजात, अखण्ड तथा सहज बन जाती है।
२८. निर्विकल्प समाधि में सोऽहं-भावना भी नहीं रहती; क्योंकि 'सोऽहं' की अनुभूति करने वाला ही कोई नहीं बचता।
२९. परम चेतना का अनुभव तुरीयावस्था है। यह निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, जिसमें परम तत्त्व के साथ ऐक्य के अपने वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान रहता है।
३०. बुद्धि के द्वार बन्द करें। इन्द्रियों के गवाक्ष बन्द करें। हृदय के कक्ष में चले जायें तथा समाधि की निद्रा-रहित निद्रा का आनन्द लें।
३१. समाधि परम चेतना की अवस्था है।
३२. समाधि ब्रह्म के साथ ऐक्य की अवस्था है।
३३. समाधि की अवस्था परमानन्द से परिपूर्ण है।
३४. समाधि की अवस्था में ध्याता अपनी व्यक्तिकता खो देता है तथा परम तत्त्व के साथ एक हो जाता है।
३५. समाधि की अवस्था अनिर्वचनीय है।
३६. सविकल्प-समाधि या सम्प्रज्ञात-समाधि में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी रहती है।
३७. सविकल्प-समाधि में संस्कार दग्ध नहीं होते।
३८. निर्विकल्प-समाधि में संस्कार पूर्णतः दग्ध हो जाते हैं।
३९. सम्प्रज्ञात-समाधि में मन के समस्त कार्य-कलापों का निरोध हो जाता है।
४०. अब योगी को कैवल्य-परम स्वतन्त्रता तथा पूर्णता की प्राप्ति होती है।
४१. परम तत्त्व के प्रति जागरूकता समाधि है।
४२. समाधि परम चेतना है। यह सभी प्रकार के द्वित्वों से परे है।
४३. (कैवल्य) समाधि में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है।
४४. समाधि में न 'मैं' रहता है, न 'तुम' और न 'वह' न 'यहाँ', न 'वहाँ', न 'यह', न 'वह', न 'ऊपर', न 'नीचे' कुछ भी नहीं रहता।
४५. समाधि परिपूर्णता, शाश्वत परमानन्द, चिरस्थायी प्रसन्नता तथा अनन्त शान्ति की अवस्था है।
४६. समाधि में आन्तरिक वा बाह्य किसी भी प्रकार के पदार्थ का भान नहीं रहता।
सविकल्प- समाधि
४७. सविकल्प समाधि में यह चेतना रहती है कि 'मैं ध्यान कर रहा हूँ, 'मेरा ध्येय है।'
४८. सविकल्प समाधि में ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की चेतना रहती है।
४९. सविकल्प समाधि में द्वित्व का भान रहता है; परन्तु वह मात्र सतही तथा आभासी होता है।
५०. सविकल्प-समाधि निर्विकल्प समाधि के लक्ष्य तक पहुँचने की तैयारी है।
निर्विकल्प समाधि
५१. निर्विकल्प समाधि की अवस्था में मन कार्य करना बन्द कर देता है; समस्त विचार शान्त हो जाते हैं; शरीर तथा बाह्य संसार की समस्त चेतना का प्रभाव मिट जाता है तथा जीवात्मा परम आत्मा में विलीन हो जाती है।
५२. समस्त संकल्पों का त्याग करके निर्विकल्प बन जायें।
५३. हमें स्वप्न में कई प्रकार के कष्टों का अनुभव होता है। जागने के बाद हमारा उन कष्टों में से किसी से भी कोई सरोकार नहीं रहता। इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि की अवस्था में या आत्मा में स्थित रहने वाला योगी प्रकृति के समस्त प्रभावों से परे रहता है।
५४. निर्विकल्प समाधि में वैयक्तिक चेतना नहीं रह जाती। यह चेतना वैश्व चेतना में विलीन हो जाती है।
५५. निर्विकल्प समाधि में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी की सत्ता निश्चित रूप से नहीं रहती।
८. प्रातिभज्ञान
१. आन्तरिक साक्षात्कार या प्रबोधन समस्त दर्शनों से परे है। यह साधक का व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव है।
२. आप केवल प्रातिभज्ञान से ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
३. प्रातिभज्ञान या आध्यात्मिक अनुभव से प्राप्त अव्यवहित ज्ञान से जीवापा तथा परमात्मा का मिलन होता है।
४. ऐन्द्रिय ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। प्रातिभज्ञान वास्तविक ज्ञान है।
५. प्रातिभज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। यह सत्य का अक्षय तथा असीम ज्ञान है।
६. अपने प्रातिभज्ञान पर आस्था रखें। यह आपको कभी निराश नहीं करेगा।
७. प्रातिभज्ञान को विकसित किये बिना बुद्धिजीवी व्यक्ति अपूर्ण ही रहता है।
८. बुद्धि सत्य की गहराइयों तक नहीं पहुँच सकती।
९. केवल प्रातिभज्ञान के द्वारा आप ब्रह्म या परम तत्त्व की झलक पा सकते हैं।।
१०. प्रातिभज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति अमर बन जाता है।
११. अपनी चतुराई और तर्क-वितर्क दे कर बदले में प्रातिभज्ञान प्राप्त करना एक लाभकारी सौदा है। तब आप शान्ति और परमानन्द को प्राप्त होंगे।
१२. विचार से प्रातिभज्ञान का द्वार खुलता है।
१३. मात्र चिन्तन की क्रिया से सत्य या परम तत्त्व उद्घाटित नहीं हो पाता।
१४. प्रातिभज्ञान के दर्शन के बिना पश्चिम का दर्शन अपूर्ण है।
१५. परम- असीम तत्व को प्रमाणित करने के वैज्ञानिक प्रयास निरर्थक है। केवल प्रातिभज्ञान ही उसे प्रमाणित करने की वैज्ञानिक पद्धति है।
१६. धार्मिक दर्शन तथा विज्ञान की समस्या का एकमात्र समाधान प्रातिभज्ञान का विकास है।
१७. वास्तविक सांस्कृतिक विकास बुद्धि से नहीं, प्रातिभज्ञान से सम्पन्न होता है।
१८. प्रातिभज्ञान, अध्यात्म के अनुभव तथा ब्रह्मज्ञान की कभी उत्पत्ति नहीं होती: क्योंकि ये अनादि काल से हैं।
१९. प्रातिभज्ञान दर्शन की एकमात्र कसौटी है।
९. समाधि तथा दिव्य अनुभव
१. निर्विकल्प - समाधि वह धन्य तथा प्रशान्त अवस्था है, जिसमें जीवन के रहस्य का उद्घाटन होता है तथा ध्याता निद्रा-रहित निद्रा में प्रवेश करता है।
२. समाधि अकर्मण्यता की अवस्था नहीं है। यह परम तत्त्व के प्रति गहन जागरूकता की अवस्था है। यह सर्वोच्च प्रातिभज्ञान है जो वस्तुओं को उनके मूल रूप में प्रकट करता है। यह शाश्वत शान्ति का अनुभव प्रदान करने वाली अवस्था है।
३. निर्विकल्प- समाधि एक आध्यात्मिक निश्चेतक है जो क्लोरोफार्म, ईथर आदि की अपेक्षा उत्तम है।
४. निर्विकल्प-समाधि में परमानुभूति होती है। समाधि आलस्य की अवस्था नहीं है। यह परम तत्त्व के प्रति जागरूकता की अवस्था है। यह सर्वोच्च प्रातिभज्ञान है।
५. जो योगी निर्विकल्प-समाधि (परम तत्त्व से ऐक्य) की अवस्था में प्रवेश कर चुका है, वह परम तत्त्व से पृथक् नहीं हो सकता ।
६. परिपूर्णता का अनुभव समाधि है। यह सभी प्रकार के द्वित्वों से परे है। अहंमन्यता तथा चिन्ताओं का इसमें कोई स्थान नहीं है। यह परम सन्तोष-प्रदायक है। इसमें इस बात की अनुभूति होती रहती है कि जो कुछ उपलब्ध करना था, वह सब उपलब्ध कर लिया है।
७. ध्यान का चरमोत्कर्ष समाधि है। समाधि-अवस्था में ध्याता परम आत्मा के साथ अपने तादात्म्य का साक्षात्कार करता है।
८. समाधि-अवस्था का अनुभव करने वाले साधक पर समाधि का प्रभाव अमिट तथा स्थायी होता है। समाधि का अनुभव प्राप्त करने वाला साधक प्रज्ञ तथा प्रबोधित बन जाता है।
९. समाधि, निर्वाण या भगवद्-दर्शन प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह केवल संन्यासियों और तपस्वियों का एकाधिकार नहीं है।
१०. समाधि-अवस्था में प्रवेश करने के लिए आसन की स्थिरता, हृदय की इन्द्रियों का प्रत्याहार तथा मन की एकाग्रता अपेक्षित है। शुद्धता,
११. समाधि पर चर्चा कर लेने या योग के ग्रन्थों का अध्ययन कर लेने से समाधि का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। आपको गम्भीरता तथा दृढ़ता से निष्ठापूर्वक योग का अभ्यास करना होगा। केवल खाना-खाना कहने से भूख समाप्त नहीं होती। बैठ कर भोजन कर लेने से ही भूख शान्त होती है। दिव्य ज्योति का प्राकट्य
१२. परम आनन्द ही परम तत्त्व है। इन्द्रिय अनुभवों के क्षेत्र से धीरे-धीरे करके ऊपर उठें और लोकोत्तर आध्यात्मिक अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश करें। जहाँ समस्त नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं, वहाँ केवल आत्मानन्द की ही सत्ता रहती है।
१३. जो सर्वव्यापी, प्रशान्त, अद्वितीय, परमानन्दपूर्ण आत्मा के दर्शन कर लेता है, उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना या जानना शेष नहीं रह जाता। इस श्रेष्ठ आत्मा को जान लें तथा शाश्वत सन्तोष एवं नित्य आनन्द प्राप्त करें।
१४. आप चाहे परम तत्त्व की झलक ही देख पायें; आपके हृदय में एक नवीन तत्त्व प्रवेश कर जाता है। सम्पूर्ण हृदय का कायापलट हो जाता है। आपका आन्तरिक व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। आप परमानन्द की लहर में निमज्जन करने लगते हैं।
१५. यदि आप ध्यानावस्था में आध्यात्मिक आनन्द की मधुरता का स्वाद एक बार भी पा जायें, तब सांसारिक पदार्थों का चिन्तन भी कर पाना आपके लिए कष्टप्रद हो जायेगा।
१६. जिसने ब्रह्म-साक्षात्कार कर लिया है, वह मौन हो जाता है। वाद-विवाद और तर्क-वितर्क का आकर्षण तभी तक रहता है, जब तक परम तत्त्व का साक्षात्कार नहीं हो जाता।
१७. जिसने ब्रह्म के परमानन्दमय स्वरूप का अनुभव कर लिया है, उसे शारीरिक अथवा मानसिक भय नहीं सताते।
१८. विषय-पदार्थों से प्राप्त होने वाला सन्तोष परावलम्बी तथा सीमित होता है। ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होने वाला सन्तोष असीमित होता है तथा किसी पर निर्भर नहीं होता।
१९. भगवद्-दर्शन एक वैश्व अनुभव है। इससे जीवन को एक नया दिग्-विन्यास प्राप्त होता है; परम तत्त्व को एक नवीन परिप्रेक्ष्य में समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह एक सम्पूर्ण अनुभव है। भगवद्-दर्शन प्राप्त साधक संसार को दिव्य विभूति की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है।
२०. भगवद्-दर्शन ध्याता की चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ता है। भगवद्-दर्शन किसी रूप का दर्शन या अनुभव नहीं है। यह प्रत्यक्ष अनुभव या प्रबोधन है।
२१. तुरीय अकथनीय ब्रह्मानन्द के मन्दिर का अन्तिम द्वार है।
२२. प्रातिभज्ञान परम साक्षात्कार की एक अपर्याप्त तथा अपूर्ण अभिव्यक्ति है। यह परम साक्षात्कार अपरोक्ष अनुभूति है ।
२३. आप अपरोक्ष अनुभूति के माध्यम से निश्चय ही सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं।
२४. अपरोक्ष अनुभूति की दीप्ति आत्मदीप्ति है। सत्य की दीप्ति प्रतिबिम्बित दीप्ति है।
२५. ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति समस्त दुःख, पीड़ाओं तथा क्लेशों का नाश करती है एवं अद्वितीय परमानन्द प्रदान करती है। शुचिता तथा ध्यान द्वारा अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त करें ।
२६. ब्रह्मैक्य से जो परमानन्द प्राप्त होता है, वह अनिर्वचनीय है। आपको स्वयं ही इसका अनुभव करना होगा।
२७. भावनाएँ तथा विचार एक ही होते हैं, परन्तु भाषाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। इसी प्रकार धार्मिक अनुभव एक समान होते हैं, परन्तु धर्म भिन्न-भिन्न होते हैं।
प्रश्नोत्तर
१. एकाग्रता का सरल मार्ग
प्रश्न : एकाग्रता का सरल मार्ग क्या है।
उत्तर : भगवन्नाम-जप करें। यह बात ध्यान में रखें कि एक दिन में पूर्ण एकाग्रता की स्थिति नहीं आती। आपको निराश नहीं होना चाहिए और न एकाग्रता के अभ्यास में ढील डालनी चाहिए। शान्त रहें; धैर्य रखें। मन इधर-उधर भटके, तब भी चिन्तित न हों । नियमित रूप से जप करते रहें। नियत समय पर ही एकाग्रता का अभ्यास करें। धीरे-धीरे मन स्वतः ही ईश्वरोन्मुख हो जायेगा। एक बार इसे ईश्वर से प्राप्त परमानन्द का स्वाद मिल जाये; फिर कोई भी इसे विचलित नहीं कर सकेगा।
२. ब्राह्ममुहूर्त में ध्यान के लाभ
प्रश्न : ब्राह्ममुहूर्त में ध्यान करने से क्या लाभ है?
उत्तर : ब्राह्ममुहूर्त में मन शान्त तथा अविक्षुब्ध होता है। इस समय यह सांसारिक विचारों, चिन्ताओं तथा परेशानियों से मुक्त रहता है। यह कोरे कागज के समान होता है तथा सांसारिक संस्कारों के प्रभावों से मुक्त होता है। इस समय मन को सांसारिक विकर्षणों के (मन में) प्रवेश करने से पूर्व ही सरलतापूर्वक ढाला जा सकता है। इस मुहूर्त में वातावरण में सत्त्व की अधिकता होती है, हलचल तथा कोलाहल भी नहीं रहता।
३. सांसारिक विचार तथा ध्यान
प्रश्न : जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ, तब मैं तरह-तरह के विचारों से घिर जाता हूँ। यह स्थिति कब समाप्त होगी ?
उत्तर : किसी बड़े शहर में सायंकाल ८ बजे बहुत हलचल तथा कोलाहल रहता है। एक घण्टे बाद हलचल और कोलाहल थोड़ा कम हो जाता है। १० बजे और भी कम हो जाता है। रात्रि ११ बजे यह बहुत कम हो जाता है। १ बजे तो सर्वत्र शान्ति छा जाती है। इसी प्रकार योगाभ्यास के प्रारम्भ में मन में अगणित वृत्तियाँ रहती हैं। मन अत्यन्त उत्तेजित तथा अशान्त हो जाता है। धीरे-धीरे विचारों की तरंगें शान्त होने लगती हैं। अन्त में मन की समस्त वृत्तियाँ नियन्त्रित हो जाती हैं। योगी परम शान्ति को प्राप्त होता है।
४. समाधि-अवस्था में प्रवेश
प्रश्न : समाधि की अवस्था में शीघ्र कैसे प्रवेश करें ?
उत्तर : मित्रों, सम्बन्धियों आदि से अपने सम्बन्ध समाप्त कर किसी से पत्र-व्यवहार न करें। अखण्ड मौन-पालन करें। एकान्त वास करें। अकेले ही विचरण करें। बहुत अल्प मात्रा में, परन्तु पौष्टिक भोजन करें। यदि हो सके, तो केवल दूध का सेवन करें। गहन ध्यान का अभ्यास करें। मन की गहराई में उतरें। निरन्तर अभ्यास करें। आप समाधि में लीन हो जायेंगे। सतर्क रहें। अपनी सहज बुद्धि का उपयोग करें। मन के साथ जोर-जबरदस्ती न करें। शिथिलीकरण की स्थिति में रहें। दिव्य विचारों को मन में धीरे-धीरे प्रवाहित होने दें।
५. भगवान् हरि तथा एकाग्रता का पदार्थ
प्रश्न : भगवान् हरि का ध्यान कैसे करें?
उत्तर : मानसिक रूप से भगवान् हरि के चरण-कमलों में मन को एकाग्र करें। फिर एक-एक करके उनके पीताम्बर, श्रीवत्स, हृदय स्थल की कौस्तुभ मणि, हाथों के कंगन, कर्णफूल, मुकुट, शंख, चक्र, गदा, पद्म और (दोबारा) चरणों पर मन को घुमायें। इसे बार-बार दोहरायें।
प्रश्न : मन को किस पदार्थ पर एकाग्र करें?
उत्तर : अपनी अभिरुचि के अनुसार अनाहतचक्र (हृदय) के कमल पर या भ्रूमध्य-बिन्दु पर ।
६. एकाग्रता
प्रश्न: मन को किस प्रकार एकाग्र किया जा सकता है ?
उत्तर : प्रारम्भ में किसी स्थूल आकार पर - हाथ में वंशी लिये हुए भगवान् कृष्ण पर या हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए भगवान् विष्णु पर मन को एकाग्र करें।
प्रश्न: किसी व्यक्ति ने मुझे परामर्श दिया है कि मैं दर्पण में अपने चेहरे के प्रतिबिम्ब के भ्रूमध्य-बिन्दु पर टकटकी लगा कर देखें। क्या मैं ऐसा कर सकता है?
उत्तर: आप ऐसा कर सकते हैं। मन की एकाग्र करने का यह भी एक तरीका है। परन्तु किसी एक ही तरीके को अपनायें। दिव्य आकारों में से किसी एक (अपने इष्टदेव) को चुन लें। यदि आप राम-भक्त हैं, तो राम का चित्र चुन लें। फिर उस पर मन को एकाग्र करें तथा उनके गुणों का ध्यान करें।
प्रश्न : लोग शालिग्राम पर एकाग्रता का अभ्यास क्यों करते हैं?
उत्तर : शालिग्राम में एकाग्रता उत्पन्न करने की क्षमता है।
प्रश्न: मैं त्रिकुटी, ॐ के प्रतीक तथा ध्वनि पर एकाग्रता का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मेरे अभ्यास ठीक है?
उत्तर: ठीक हैं। शुचिता, सत्, चित् तथा आनन्द के विचारों को ॐ के साथ : सम्बद्ध कर लें। यह अनुभव करें कि आप सर्वव्यापक चेतना हैं। इस प्रकार का भाव आवश्यक है।
प्रश्न: गहन एकाग्रता की स्थिति में प्रवेश करने के लिए क्या करूँ?
उत्तर: गहन मानसिक वैराग्य विकसित करें। अभ्यास की अवधि बढ़ा दें। एकान में बैठें। अवांछनीय व्यक्तियों से अधिक मेल-जोल न रखें। प्रतिदिन तीन घण्टे तक मौन रखें। रात्रि के समय दूध तथा फलों का सेवन करें। आप गहन एकाग्रता की स्थिति में प्रवेश कर सकेंगे।
प्रश्न: शिष्य को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। कभी-कभी वह गुरु के सम्पर्क में आना चाहता है। इसीलिए मैं आपको पत्र लिख कर आपकी शान्तिं भंग किया करता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एकाग्रता-क्षमता का विकास किस प्रकार होता है?
उत्तर: आप मुझे कभी-कभी पत्र लिख सकते हैं। शान्ति भंग होने का सम्बन्ध मन से है। आत्मा (जो मन के भी परे है) में ही सुस्थित रहने वाले व्यक्ति के लिए सदैव शान्ति ही शान्ति है। ऐसे आत्म-स्थित व्यक्ति को मानसिक विक्षोभ, कष्ट, मनस्ताप प्रभावित नहीं कर पाते। कामनाओं को कम कर देने से, प्रतिदिन दो घण्टे तक मौन रहने से, नित्व एक-दो घण्टे तक किसी शान्त कक्ष में एकान्त-वास करने से, प्राणायाम का अभ्यास करने से, प्रार्थना करने से, सायंकाल और रात्रि के समय ध्यान करने के लिए अधिक बार बैठने से तथा विचार (जिज्ञासा) करने से एकाग्रता का विकास होता है।
प्रश्न: क्या जप से एकाग्रता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ?
उत्तर: हाँ, मानसिक जप किया करें।
प्रश्न: जब मैं त्रिकुटी पर एकाग्र होने का प्रयास करता हूँ, तब मुझे थोड़ा शिर-दर्द होने लगता है। इसका क्या उपचार है?
उत्तर : मन के साथ लड़ाई न करें। एकाग्रता का अभ्यास करते समय मन पर अत्यधिक जोर न डालें। अपनी समस्त नाड़ियों, पेशियों तथा मस्तिष्क को शिथिल करें। सहज, स्वाभाविक ढंग से मृदुल एकाग्रता का अभ्यास करें। इससे मन पर आवश्यक रूप से पड़ता हुआ जोर समाप्त हो जाता है। शिर-दर्द भी मिट जायेगा।
प्रश्न : मेरा मन अभी भी चंचल है और मुझमें विषयासक्ति की दुर्बलता है। एकाग्रता के अभ्यास में कभी-कभी सफलता प्राप्त होती है; परन्तु अन्त में निराशा ही हाथ लगती है। मन का शुद्धिकरण सरल नहीं है। कृपया परामर्श दें।
उत्तर : आपका वैराग्य शुद्ध नहीं है। वैराग्य का विकास करें। गहन साधना करें। अपनी साधना का समय बढ़ा दें और चार घण्टे तक अभ्यास करें। अपने व्यवहार (कर्म आदि) को कम करें। ऋषिकेश या उत्तरकाशी जा कर तीन महीने तक एकान्त वास करें। पूरे तीन महीने तक मौन रखें। आपके एकाग्रता तथा ध्यान आश्चर्यजनक रूप से गहन हो जायेंगे।
प्रश्न: जो योगी अपने शिष्य पर शक्ति संचार करता है, वह क्यों उससे अन्य सभी प्रकार की साधनाएँ छोड़ देने को कहता है ?
उत्तर : ताकि शिष्य गहन आस्था का विकास कर सके, अपने साधना-मार्ग पर दृढ़ रह सके तथा किसी एक ही प्रकार के योग में एकाग्र मन से श्रद्धा रख सके।
प्रश्न: मैं प्रतिदिन दो घण्टे तक जप तथा आधे घण्टे तक प्राणायाम करता हूँ। क्या मैं दो या तीन वर्षों के अन्दर एकाग्रता और अनन्यता प्राप्त कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, यदि आप शुद्ध हृदय से अपनी साधना के प्रति निष्ठावान् हैं, तो यह सम्भव है।
७. ध्यान
प्रश्न : ब्राह्ममुहूर्त क्या है?
उत्तर : प्रातः काल ४ बजे का समय ब्राह्ममुहूर्त है।
प्रश्न : ऋषि-मुनियों ने ब्राह्ममुहूर्त की इतनी प्रशंसा क्यों की है ?
उत्तर : क्योंकि यह समय ब्रह्म ध्यान के लिए अत्यन्त उपयुक्त है, इसीलिए इसे ब्राह्ममुहूर्त कहा जाता है।
प्रश्न : ब्राह्ममुहूर्त में ध्यान करने से क्या लाभ होते हैं?
उत्तर : इस समय मन शान्त तथा अविक्षुब्ध होता है एवं सांसारिक विचारों, चिन्ताओं और परेशानियों से मुक्त रहता है। इस समय मन कोरे कागज की तरह होता है या सांसारिक संस्कारों के प्रभावों से मुक्त रहता है। इस समय ध्यान करने से मन को उसमें सांसारिक विकर्षणों के प्रवेश करने से पहले ही सरलतापूर्वक ढाला जा सकता है। अन्य समयों की अपेक्षा ब्राह्ममुहूर्त में वातावरण अधिक सत्त्व से आवेशित रहता है। इस समय वातावरण में कोलाहल भी नहीं होता।
प्रश्न : ध्यानाभ्यास प्रारम्भ करने से पूर्व क्या मुझे स्नान कर लेना चाहिए?
उत्तर : यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तथा मौसम प्रतिकूल नहीं है तथा आप चुस्त हैं, तो आप इच्छानुसार ठण्ढे, गुनगुने या गरम पानी से स्नान कर सकते हैं, अन्यथा ठण्डे पानी से हाथ, पैर और मुँह धो लेना ही पर्याप्त होगा। ध्यान करने से पहले आचमन भी करें। आचमन का अर्थ है— दाहिने हाथ में जल ले कर 'अच्युताय नमः ॐ', 'अनन्ताय नमः ॐ', 'गोविन्दाय नमः ॐ' मन्त्र पढ़ कर शुद्धि के निमित्त मुँह में जल लेना ।
प्रश्न: ध्यान (या मन को एकाग्र) कैसे करें?
उत्तर : प्रारम्भ में एक वर्ष तक चार भुजाओं वाले भगवान् हरि पर मन को एकाग्र करें। तब किसी विचार का अमूर्त ध्यान करें, यथा-ॐ एक, अखण्ड चिदाकाश, सर्वभूत, अन्तरात्मा ।
प्रश्न: मन को एकाग्र करना ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। ध्यान के समय मन प्रायः सदैव ही चंचल हो जाता है। क्या उपाय है?
उत्तर : अपने वैराग्य और अभ्यास को दृढ़ करें। लक्ष्य पर मन को बार-बार लायें । यदि मन ५५ बार भटकता है और किसी दिन आप इसे ५० बार ही भटकने दें, तब भी यह एक उपलब्धि है। जाड़े के मौसम में मौन रहने से बहुत लाभ होता है। प्रातः, सन्ध्या तथा रात्रि के समय ध्यान के लिए बैठें। अपराह्न,
प्रश्न: ध्यान करते समय मन स्फूर्तिहीन और सुस्त होने लगता है। उस समय मन उन्नत बनाने के लिए (प्राणायाम के अतिरिक्त) क्या उपाय करूँ? क्या मैं 'प्रतिकूल सुझाव' की विधि अपना सकता हूँ?
उत्तर: जब भी मन की ऐसी स्थिति हो, तो दृढतापूर्वक कहें- 'मैं आत्मा हूँ। मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं ज्ञान-स्वरूप हूँ। मैं सर्वशक्तिमान् हूँ — ॐ ॐ ॐ ।' तब मन उन्नत हो जायेगा तथा (ध्यान के लिए) केन्द्रित हो जायेगा।
प्रश्न : एक योगी ने मुझे बताया कि ईश्वर का ध्यान करते समय उसे कृष्ण की बाँसुरी की ध्वनि तथा शंखनाद सुनायी पड़ते हैं। क्या यह सत्य है ? यदि हाँ, तो इन ध्वनियों को किस प्रकार सुना जा सकता है?
उत्तर : यह बात बिलकुल सच है। कृष्ण के चित्र पर मन को टिकायें। आपको ये दोनों प्रकार की ध्वनियाँ सुनायी पड़ेगी। अपने कानों को हाथ के दोनों अँगूठों से बन्द कर लें या पीली मधुमक्खी के मोम के साथ बने हुए रूई के गोलों से भी कानों को ढक सकते हैं। दाहिने कान से सुनायी पड़ने वाली ध्वनियों पर मन को गहन रूप से एकाग्र करें। यह अभ्यास रात्रि के समय करें। आपको ये ध्वनियाँ सुनायी पड़ेंगी।
प्रश्न : निवेदन है कि मुझे कुछ और अधिक निर्देश दें। ध्यान की कुछ और विधियाँ बतायें। सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कुछ स्पष्ट संकेत भी दें।
उत्तर : भगवान् कृष्ण के शरीर के प्रत्येक भाग का मानस-दर्शन करें। उनके पीताम्बर, बाँसुरी आदि को भी मन की आँखों से देखें। इन बिम्बों को स्थिर रखने का प्रयत्न करें। मन भटकने लगेगा, तो इसे वापस लाना कठिन होगा। अतः इसे कुछ देर तक भटकने दें। इधर-उधर उछल-कूद मचाने के बाद यह स्वतः शान्त हो जायेगा।
प्रश्न: हम ध्यान के लिए अपना समय क्यों दें? भगवान् को हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है।
उत्तर : जीवन का लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार या भागवती चेतना की अनुभूति करना । हमारे सब दुःख, जन्म, जरा, मृत्यु मात्र ब्रह्म-साक्षात्कार से ही समाप्त हो सकते हैं। ईश्वर का ध्यान करके उसका साक्षात्कार हो सकता है। प्रिय राम! इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अतः ध्यानाभ्यास करें। भगवान् हमें प्रार्थना, जप आदि करने के लिए प्रेरित करते हैं; क्योंकि वह हमारे मन के प्रेरक हैं।
प्रश्न: ध्यान करते समय क्या मैं ईश्वर से सहायता प्राप्त कर सकता हूँ?
उत्तर : हाँ, आपके हृदय में प्रकाशित ईश्वरीय सत्ता दोनों हाथ फैला कर सच्चे भक्तों का आलिंगन करने के लिए तत्पर है।
प्रश्न: क्या रात्रि में भोजन के उपरान्त ध्यान करना चाहिए? गृहस्थों के पास सन्ध्या-समय बहुत से काम रहते हैं। इस कारण वे सन्ध्या के समय ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाते।
उत्तर : रात्रि के समय ध्यान करना अति आवश्यक है। यदि रात्रि को ध्यान करने का पर्याप्त समय आपके पास नहीं है, तो सोने से पूर्व मात्र १०-१२ मिनट तक ही ध्यान करें। इस प्रकार आपके आध्यात्मिक संस्कारों में वृद्धि होगी। आपके आध्यात्मिक संस्कार आपकी अत्यन्त मूल्यवान् सम्पत्ति हैं। इससे एक लाभ यह भी होगा कि रात्रि में आप बुरे स्वप्न नहीं देखेंगे। दिव्य विचारों का प्रभाव निद्रावस्था में भी बना रहेगा। उस अवस्था में अच्छे संस्कारों का भी प्रभाव रहेगा।
प्रश्न : जप और ध्यान में क्या अन्तर है?
उत्तर : जप भगवन्नाम की निःशब्द आवृत्ति है। ध्यान ईश्वर के एकमात्र विचार का अनवरत प्रवाह है। जब आप 'ॐ नमो नारायणाय' को बार-बार दोहराते हैं, तब यह विष्णु-मन्त्र का जप कहलाता है, और जब आप विष्णु भगवान् के शंख, चक्र, गदा तथा पद्म, कर्णफूलों, मुकुट, कौशेय पीताम्बर आदि का चिन्तन करते हैं, तब यह ध्यान है। जब आप उनके गुणों— सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि के बारे में सोचते हैं, तब भी यह ध्यान है।
प्रश्न: कृपया ध्यान करने से सम्बन्धित कुछ व्यावहारिक निर्देशन दें।
उत्तर : एकान्त कक्ष में पद्मासन या सिद्धासन में बैठें। शिर, गरदन तथा धड़ को एक सीध में रखें। नेत्र बन्द कर लें। सोचें कि आपके हृदय में एक बहुत बड़ा देदीप्यमान सूर्य प्रकाशित हो रहा है। मानसिक रूप से कमल के फूल के बीचों-बीच भगवान् विष्णु के चित्र को रखें तथा उस फूल को उस सूर्य के केन्द्र में स्थापित करें। उनके मन्त्र-ॐ 'नमो नारायणाय' का मानसिक जप करें। उनके चरणों से ले कर शिर तक की शंख, चक्र, गदा, पद्य आदि लिये हुए पूरी आकृति का अपने हृदय में मानस-दर्शन करें। अन्य किसी प्रकार के सांसारिक विचारों का चिन्तन न करें।
प्रश्न: जब मैं ध्यान करता हूँ, तब मेरा शिर भारी हो जाता है। मैं क्या करूँ ?
उत्तर: शिर में आंवले का तेल लगायें तथा ठण्डे पानी से स्नान करें। ध्यान करने से पहले शिर पर ठण्डे पानी के छींटे डालें। आप इस समस्या से मुक्त हो जायेंगे मन के साथ जोर-जबरदस्ती न करें।
प्रश्न: क्या एकान्तवास आवश्यक है ?
उत्तर : बिलकुल आवश्यक है। यह एक अपरिहार्य आवश्यकता है।
प्रश्न: मुझे कितनी अवधि तक एकान्त वास करना चाहिए?
उत्तर : पूरे तीन वर्षों तक ।
प्रश्न: ध्यान करने के लिए कुछ एकान्त स्थानों के नाम बतायें।
उत्तर : ऋषिकेश, हरिद्वार, नासिक, उत्तरकाशी, बदरीनारायण, कनखल (हरिद्वार में), वृन्दावन, मथुरा, अयोध्या और कश्मीर ।
प्रश्न: चिन्तनमय जीवन के लिए मैं अपने को कैसे तैयार करूँ?
उत्तर : अपनी सम्पत्ति को अपने पुत्रों में बाँट दें। अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचा कर रखें। सम्पत्ति के कुछ अंश का दान कर दें। ऋषिकेश में कुटीर बना कर रहें। अपने पुत्रों से पत्र-व्यवहार न करें। मैदानी क्षेत्रों में न जायें। ध्यानाभ्यास प्रारम्भ करें। तब आपके मन को शान्ति मिलेगी। इसे तुरन्त ही कार्यान्वित करें। शीघ्रता करें।
प्रश्न : जब मैं उत्तरकाशी में था, तब मुझमें निष्ठा थी, उदात्त वृत्तियाँ थीं तथा मैं धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहा था। मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद मुझमें ये गुण नहीं रह गये हैं, यद्यपि मैं अब भी साधना करता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? पूर्व की भाँति बनने के लिए मैं क्या करूँ?
उत्तर : सांसारिक व्यक्तियों का सम्पर्क तुरन्त ही मन को प्रभावित करता है। मन में विक्षेप आ जाता है। मन (सांसारिक व्यक्तियों का) अनुकरण करने लगता है। बुरी तथा राजसी आदतें विकसित हो जाती हैं। खराब वातावरण तथा कुसंग का साधक के मन को बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ होता है। पुराने संस्कार फिर प्रभावी हो जाते हैं। आप तुरन्त ही उत्तरकाशी वापस चले जायें। एक मिनट का भी विलम्ब न करें। भोजन के सूक्ष्मतम अंश से मन का निर्माण होता है, इसीलिए जिस व्यक्ति का दिया हुआ भोजन खाया जाता है, मन उसी व्यक्ति में आसक्त हो जाता है। किसी व्यक्ति के नैतिक बन्धन में न रहें। स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करें। अपने पर ही भरोसा रखें।
प्रश्न: पिछले छह वर्षों से ध्यान का अभ्यास करते रहने पर भी मुझे ध्यान में सफलता क्यों नहीं मिल रही है ?
उत्तर : आपका चित्त शुद्ध नहीं है।
प्रश्न : मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा चित्त शुद्ध है कि नहीं ?
उत्तर: चित्त शुद्ध होने पर कामुक विचार तथा वासनाएँ, सांसारिक कामनाएं, अपवित्र विचार, क्रोध, मिथ्याभिमान, दम्भ, अहंभाव, लोभ, ईर्ष्या आदि विकार मन में उत्पन्न नहीं होंगे। तब विषय-पदार्थ आपको आकर्षित नहीं कर पायेंगे। आपका वैराग्य-भाव अखण्ड तथा चिरस्थायी बन जायेगा। स्वप्न में भी आप बुरे विचारों का स्वागत नहीं करेंगे। आपमें करुणा, वैश्व प्रेम, क्षमाशीलता, सामंजस्य तथा मानसिक सन्तुलन के दिव्य सद्गुणों का उदय होगा। जब ऐसा हो जाये, तब समझ लें कि आपका चित्त शुद्ध हो गया है।
प्रश्न: चित्त को शुद्ध करने में कितना समय लगता है?
उत्तर : यह साधक के क्रम विकास तथा उसकी साधना के स्तर पर निर्भर करता है। प्रथम श्रेणी के साधक को अपना चित्त शुद्ध करने में छह माह ही लगेंगे। मध्यम श्रेणी के साधक को इस कार्य के लिए ४ वर्ष लग सकते हैं।
८. समाधि
प्रश्न : समाधि क्या है?
उत्तर : यह ब्रह्म के साथ ऐक्य की स्थिति है।
प्रश्न : तुकाराम, तुलसीदास, रामदास तथा अन्य भक्तों ने किस प्रकार की समाधि की अवस्था में प्रवेश किया था ?
उत्तर: सविकल्प समाधि में।
प्रश्न : क्या सविकल्प-समाधि-प्राप्त ऐसे साधकों में वासनाएँ हो सकती हैं?
उत्तर : नहीं।
प्रश्न: उनकी स्थिति क्या होती है?
उत्तर: भगवद्-साक्षात्कार प्राप्त ऐसे भक्त ईश्वरैक्य की स्थिति में होते थे परन्तु उनकी वैयक्तिकता उनसे एक झीने आवरण से जुड़ी रहती थी। उन्हें समस्त दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त थे। वे सभी प्रकार की सांसारिक विपत्तियों से पूर्णतः मुक्त थे। वे दिव्य परमानन्द में निम रहते थे। वे अपने कारण शरीर से ही क्रियाशील होते थे।
प्रश्न: निर्विकल्प समाधि क्या है?
उत्तर : यह एक सर्वोच्च चेतना की स्थिति है, जिसमें जीवात्मा ब्रह्म के साथ मिल कर एक हो जाता है।
प्रश्न : महासमाधि क्या है ?
उत्तर : निर्विकल्प-समाधि तथा महासमाधि एक ही हैं।
प्रश्न: तुरीयावस्था क्या है?
उत्तर : यह समाधि की वह अवस्था है, जिसमें साधक निज-स्वरूप अथवा ब्रह्म में स्थित रहता है। यह उच्च चेतना की वह स्थिति है, जिसमें ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है। एक रूसी दार्शनिक के अनुसार यह चतुर्थ आयाम है।
प्रश्न: तुरीयावस्था में कैसे प्रवेश किया जा सकता है?
उत्तर : विचार, वासना क्षय तथा मनोनाश के द्वारा ।
प्रश्न: समाधि-अवस्था में शीघ्र प्रवेश करने के लिए क्या करें?
उत्तर : अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से सारे सम्बन्ध समाप्त कर लें। एक माह तक अखण्ड मौन का पालन करें। एकान्त में रहें। अल्प मात्रा में, परन्तु पौष्टिक भोजन लें। यदि सम्भव हो सके, तो केवल दुग्धाहार करें। गहन ध्यान करें। मन की गहराइयों में उतरें। निरन्तर अभ्यास करें। आप समाधि की स्थिति में तल्लीन हो जायेंगे। जागरूक रहें। अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करें। मन के साथ जबरदस्ती न करें। तनाव रहित स्थिति में रहें। अपने मन में दिव्य विचारों को धीरे-धीरे प्रवाहित होने दें।
प्रश्न: क्या निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रवेश करना तथा इस अवस्था में - सांसारिक कार्य-कलापों से मुक्त होना वास्तव में सम्भव है?
उत्तर : बिलकुल सम्भव है। यदि आप प्रतिदिन छह घण्टे तक ध्यान करें, तो आप निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। आत्म-विश्लेषण करें तथा अहंकार, लोभ, कामुकता, मोह तथा आसक्ति के समस्त सूक्ष्म रूपों से अपने को मुक्त रखें।
प्रश्न: क्या आप किसी ऐसे योगी के बारे में जानते हैं जो प्राणायाम द्वारा समाधि की स्थिति में कुछ महीनों तक रह सकता हो ?
उत्तर : नहीं।
९. मन्त्र - साधना के अनुभव
प्रश्न : यह कैसे पता चले कि मन्त्र जप से साधक लाभान्वित हो रहा है?
उत्तर : जो साधक मन्त्रयोग का अभ्यास कर रहा है, वह प्रत्येक समय भगवान् की उपस्थिति का अनुभव करेगा। वह अपने हृदय में दिव्य प्रहर्ष तथा पावन पुलक का भी अनुभव करेगा। उसके मन तथा हृदय शुद्ध हो जायेंगे। वह रोमांचित हो उठेगा। वह प्रेम के आँसू बहायेगा तथा ईश्वर के पवित्र सम्पर्क में रहेगा।
१०. प्रातिभज्ञान की विधि
प्रश्न: क्या दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रातिभज्ञान की विधि को विश्वसनीय माना जा सकता है?
उत्तर : 'प्रातिभज्ञान की विधि' यह वाक्यांश भ्रामक है। इससे यह भ्रम उत्पन्न होता है कि सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने की अनेक विधियों में से यह भी एक विधि है। वस्तुतः प्रातिभज्ञान ही एकमात्र अतार्किक बाह्यानुभूति है। पूर्णतः तर्कसंगत ज्ञान बुद्धि तथा तर्क के परे नहीं जा पाता, अतः वह प्रातिभज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट है। जब तक प्रातिभज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक तार्किक ज्ञान श्रेष्ठ प्रतीत होता है। पश्चिम में भी, जहाँ व्यवहार्य प्रमाण्य ज्ञान को ही महत्व दिया जाता है, दार्शनिक प्रातिभज्ञान के महत्व को समझने लगे हैं। वे मनुष्य को सम्यक् ज्ञान उपलब्ध कराने में इसकी (प्रातिभज्ञान की भूमिका के सही-सही मूल्यांकन की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो गये हैं।
११. सहज समाधि तथा निर्विकल्प-समाधि
प्रश्न
१. सहज-समाधि क्या है? निर्विकल्प समाधि से इसका क्या सम्बन्ध है?
२. सहज-समाधि में श्वास तथा सोऽहं की क्या भूमिका होती है? क्या सहज समाधि की अवस्था में योगी के लिए संसार का अस्तित्व रहता है?
३. श्रीरामकृष्ण-जैसे महान् सन्तों ने कहा है कि निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करने के पश्चात् योगी केवल २१ दिन तक जीवित रहता है। कृपया इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें।
४. जब सहज-समाधि में ही सुख और सन्तोष मिल जाते हैं, तब निर्विकल्प समाधि के लिए प्रयत्न क्यों करें ?
उत्तर :
समाधि का ही विस्तार सहज समाधि है। इसका प्रभाव दिन में चौबीसों घण्टे रहता है (न केवल उसी समय जब योगी ध्यान के लिए बैठता है)। 'ईश्वर की सत्यता', 'नाम-रूपों की असत्यता' तथा इस तथ्य का आन्तरिक साक्षात्कार कि 'जीवात्मा सर्वव्यापी परमात्मा ही है'-इन तीनों का बोध सहज-समाधि में रहता है। जिस समाधि की अवस्था में साधक प्रथमतः बहिरंग-साधना द्वारा तथा फिर अन्तरंग साधना द्वारा प्रवेश करने का प्रयास करता है, वह सहज बन जाती है। अहं, संसार तथा साधक का अपना शरीर उस शीशे की तरह दिखायी पड़ने लगते हैं, जिस पर आर्द्रता की मोटी परत जम जाती है। आप उस शीशे के दूसरी ओर देख सकते हैं; परन्तु आर्द्रता की परत के कारण (जिसके परिणाम स्वरूप उसमें अपारदर्शिता थोड़ी रह जाती है) वह शीशा भी दिखायी पड़ता है। सहज समाधि की अवस्था में योगी संसार को उस मनुष्य के समान देखता है जो यह जानता है कि मृगमरीचिका मृगमरीचिका ही है, जल नहीं।
सहज समाधि में योगी में अहं का किंचित् सात्त्विक अंश रहता है। इसी के कारण - वह संसार में रहता हुआ कार्य करता है तथा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है; परन्तु सोऽहं में सुस्थित रहने के कारण संसार में रहने, कर्म करने तथा अनुभव प्राप्त करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता के द्वितीय अध्याय में स्थितप्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान् श्री कृष्ण ने यही बात कही है।
१२. सहज समाधि की सुरभि -
प्रश्न : सहज समाधि से निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? सहज समाधि इसमें क्योंकर सहायक होती है?
उत्तर : सहज समाधि से निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करने के लिए साधक को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। यदि योगी कोई प्रयास करता भी है, तो वह सहज अवस्था में बने रहने के लिए ही ऐसा करता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका अल्प सात्त्विक अहंभाव राजसिक न बनने पाये। यद्यपि इस प्रकार का पतन बहुत कम होता है; परन्तु धर्मग्रन्थों में ऐसे विवरण पढ़ने को मिल जाते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि थोड़ी-सी भी असावधानी सारा खेल बिगाड़ देती है। जैसा कि गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है- "यदि साधक अपने जीवन के अन्त तक़ (जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता) सहज अवस्था को बनाये रखे, तो वह ब्रह्म-निर्वाण या निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होता है।" -
सहज-समाधि भागवती-चेतना की अवस्था होती है। योगी इस अवस्था में सक्रिय होकर लोक-संग्रह करता है। निष्काम सेवा तथा वैश्व प्रेम में कर्म शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं तथा दिव्य परमोत्कर्ष का बिन्दु शीघ्रता से निकट आने लगता है। साथ ही साथ सहज अवस्था से किंचित् भी अधोगमन होने का खतरा समाप्त हो जाता है।
१३. समाधि में अनुभव
प्रश्न : समाधि में क्या-क्या अनुभव होते हैं?
उत्तर : समाधि के अनुभव वर्णनातीत हैं। भाषा समाधि के अनुभवों का विवरण पूर्णतः प्रस्तुत नहीं कर पाती। जिस प्रकार मिसरी खाने वाला मिसरी के स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता, उसी प्रकार योगी अपने अनुभव दूसरों को नहीं बतला पाता। समाधि का अनुभव योगी अपने अन्तर्ज्ञान से करता है। समाधि-अवस्था में योगी अन्ततः परमानन्द का अनुभव करता है तथा परम ज्ञान प्राप्त करता है।
प्रश्न : समाधि में हम क्रम से क्या-क्या देखते और अनुभव करते हैं?
उत्तर : समाधि में क्रम योग के प्रकार के अनुसार बदलते रहते हैं। भक्त को शुद्ध मन और भक्ति से भाव-समाधि तथा महाभाव-समाधि प्राप्त होती है। भक्त श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, रुचि, रति, स्थायी भाव तथा महाभाव के प्रक्रमों से हो कर गुजरता है। राजयोगी विचारों के दमन तथा संयम द्वारा सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, सस्मिता सानन्द तथा फिर असम्प्रज्ञात-समाधि को प्राप्त होता है। उसे ऋतम्भरा प्रज्ञा, मधुभूमिका, धर्ममेघ, प्रसंख्यान आदि की प्राप्ति होती है। ज्ञानी या वेदान्ती को अन्तर्दृष्टि, प्रातिभज्ञान, सत्योद्घाटन तथा प्रबोधन प्राप्त होते हैं। उसे प्रहर्ष तथा परमानन्द का अनुभव होता है। वह मोह, अहंकार, शून्यता, अनन्त आकाश, बोध तथा बोधाभाव से राहित्य, अनन्त चेतना तथा परमानन्द की अवस्थाओं से होता हुआ आगे बढ़ता है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसी, सत्वापति, असंसक्ति, पदार्थाभावना तथा तुरीय वेदान्ती की सात भूमिकाएं हैं। ज्ञानयोगी हमेशा समाधि-अवस्था में रहता है। उसके लिए समाधि में प्रविष्ट अथवा उससे उत्थित होने जैसी कोई अवस्था नहीं है।
१४. मनन तथा अतिचेतनावस्था का अनुभव
प्रश्न: मनन और ध्यान में क्या अन्तर है?
उत्तर : सुनी हुई बात पर चिन्तन या विचार करना मनन है। मन में केवल ब्रह्म का ही विचार बनाये रखना ध्यान है। मनन का परिणाम ध्यान है। ध्यान का परिणाम समाधि है।
प्रश्न: क्या योगी निर्विकल्प समाधि से स्वेच्छा से बाहर आ सकता है ?
उत्तर : हाँ।
प्रश्न: क्या समाधिस्थ व्यक्ति को अन्य लोग भ्रम से मृत अथवा विनाश प्राप्त समझ सकते हैं?
उत्तर : हाँ।
प्रश्न: ध्यान और पूजा में क्या अन्तर है ?
उत्तर : पुष्पार्पण, आरती, भजन आदि पूजा के अंग हैं। मन में ईश्वर या आत्मा के ही एकमात्र विचार के सतत प्रवाह को बनाये रखना ध्यान है।
१५. रहस्यवादियों के अनुभव
प्रश्न: कुछ साधक कहते हैं कि उन्हें ध्यान में ज्योति दिखलायी पड़ती है तथा अनाहत स्वर सुनायी पड़ते हैं। क्या यह सही है?
उत्तर : ये सब एकाग्रता की प्रथम अवस्था के लक्षण हैं।
प्रश्न : कृपया निर्विकल्प समाधि का वर्णन करें।
उत्तर: यह वर्णनातीत है। यह साधक के व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवों की अवस्था है। इस अवस्था में परम शान्ति तथा परमानन्द का अनुभव होता है। क्या कोई मिसरी या सेब के स्वाद का वर्णन कर सकता है?
प्रश्न: इस अन्तिम अवस्था, समाधि में कैसे प्रवेश करें?
उत्तर : अपने हृदय शुद्ध करें। ध्यान करें। आप समाधिस्थ हो जायेंगे।
प्रश्न: हमें यह कैसे पता चले कि रहस्यवादियों तथा सन्तों के अनुभव सत्य है?
उत्तर : उनके शब्दों में एक शक्ति होती है। उनका सम्पर्क उन्नयनकारी तथा प्रेरणादायक होता है। वे सदैव शान्ति, आह्लाद तथा परमानन्द से परिपूर्ण रहते हैं। वे कामुकता, , लोभ, क्रोध तथा रुचि अरुचियों से मुक्त रहते हैं। उनके अनुभव गीता तथाउपनिषदों में वर्णित सन्तों के अनुभवों के अनुरूप होते हैं।
१६. प्रज्ञा का दिव्य नेत्र - प्रातिभज्ञान
प्रश्न: मैं विचार-शक्ति तथा इससे सम्बन्धित आपके अनुभवों के बारे में जानना चाहता हूँ।
उत्तर : मन को एकाग्र करके बैठ जायें। नेत्र बन्द कर लें। आपको विचार सम्प्रेषण (thought-transference) का अनुभव होगा।
प्रश्न: आप प्रातिभज्ञान को किस प्रकार परिभाषित करेंगे?
उत्तर : प्रातिभज्ञान एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह प्रज्ञा का दिव्य नेत्र है।
प्रश्न : कल्पना करें कि मैं किसी को १०० रुपये देना चाहता हूँ, परन्तु मैं निर्धन हूँ। रुपये देने के लिए हृदय तो तड़प रहा है; परन्तु तर्क-शक्ति इसके लिए मना करती है। क्या यह प्रातिभज्ञान है ?
उत्तर : यह प्रातिभज्ञान का उदाहरण नहीं है।
प्रश्न: क्या आप यह मानते हैं कि प्रातिभज्ञान की सहायता से किये गये कार्य सदैव ठीक और सही होते हैं?
उत्तर : हाँ, योगी के ऐसे कार्य त्रुटिरहित होते हैं; क्योंकि वह दिव्य या परम प्रज्ञा के सम्पर्क में रहता है।
परिशिष्ट१
समाधि तथा आध्यात्मिक अनुभव
१. पदार्थों से मन को हटा लें अपने अन्तरतम की गहराइयों में कूद जायें और आत्म-स्थित हो जायें ।
२. समाधि की अवस्था में समस्त नाम रूपों का लोप हो जाता है। उसमें होता है। एक असीम, अनन्त, चेतन प्रकाश का सागर ।
३. रूप छायाओं अथवा कैन्वस पर बने चित्रों की तरह अवास्तविक प्रतीत होते हैं।
४. दिशा तथा काल का लोप हो जाता है। अहंभाव मिट जाता है। समस्त प्रकार के द्वित्व समाप्त हो जाते हैं।
५. आत्मपरक तथा वस्तुपरक का सम्बन्ध समाप्त हो जाता है।
४. एकमात्र अनन्त शून्यता का अनुभव होता है।
७. 'अहमस्मि' का अनुभव होता है।
८. फिर सच्चिदानन्द का अनुभव होता है।
९. तब केवल सन्मात्र अवशेष रह जाता है। आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है।
१०. निर्विकल्प समाधि में गहन परमानन्द का अनुभव होता है।
परिशिष्ट २
ध्यान के लिए सूक्तियाँ
१. शुद्ध और स्थिर मन में ही प्रज्ञा का उदय होता है; अतः अपने मन को शुद्ध करें और शान्त हो जायें ।
२. ध्यान की बाधाएँ हैं—निद्रा, कामुकता, अस्थिरता और दिवास्वप्न ।
३. ब्रह्म स्थूल चिन्तन से परे है; परन्तु शुद्ध, सूक्ष्म और एकाग्र मन से ध्यान की स्थिति में उसका साक्षात्कार किया जा सकता है।
४. सन्तों के जीवन मोक्ष मार्ग के दिक्सूचक हैं।
५. कडुवी औषधि का ही अपेक्षित प्रभाव होता है।
६. अभ्यास ही ईश्वर-साक्षात्कार का सरलतम, संक्षिप्त और असन्दिग्ध उपाय है और यह अभ्यास है— सर्वव्यापक ईश्वर का ध्यान ।
७. निःस्वार्थ सेवा जीवन का नमक, समस्त जीवों के प्रति प्रेम जीवन की रोटी और शुद्धता जीवन का जल है।
८. पूर्ण आत्म-समर्पण जीवन की मधुरता है। उदारता जीवन की सुगन्धि है। ध्यान जीवन का आधार है। आत्म-साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य है।
९. ध्यान के फल हैं—आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति, पूर्ण शान्ति, साक्षात्कार तथा परमानन्द ।
१०. जो व्यक्ति काम-क्रोध का गुलाम है, वह पशुओं से भी गया-बीता है।
११. क्रोध अज्ञानता का पुत्र, ईर्ष्या का भाई तथा निष्ठुरता का जनक है।
१२. जो जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, वह रीता है, व्यर्थ है।
१३. समर्पण जीवन की धारा है, एक प्रचण्ड शक्ति है।
१४. आत्म-समर्पण मुक्ति और शान्ति का प्रदाता है। यह कष्टों को समाप्त करता है।
१५. आध्यात्मिक विकास क्रमिक और धीरे-धीरे होता है। शीघ्रता से सब कुछ कर डालने का प्रयत्न न करें। दो-तीन महीनों में ही पूर्णता को प्राप्त करने की आशा न रखें।
१६. योग की निःश्रयणी पर एक-एक डण्डा करके चढ़ें। एक-एक कदम बढ़ाते हुए ही अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
१७. प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है।
१८. प्रार्थना पहाड़ों को हिला सकती है; परन्तु प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए।
१९. आप नाशवान् शरीर नहीं हैं। आपकी सत्ता आत्मा का सार है। आप आत्मा से अभिन्न है।
२०. सन्तत्व के लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग है नियमित ध्यान । यम और नियम सन्तत्व की आधारशिलाएँ हैं।
२१. समस्त जीवों के प्रति प्रेम सन्तत्व का प्रकाश है। सद्गुण सन्तत्व के परिधान हैं। प्रत्येक वस्तु के प्रति समान श्रद्धा इसका लक्षण है।
२२. भगवद्-दर्शन या आत्म-साक्षात्कार से बढ़ कर इस संसार में कोई भी प्रकाश नहीं है।
२३. सन्तोष से बढ़ कर और कोई धन नहीं है।
२४. सत्य से बढ़ कर और कोई सद्गुण नहीं है।
२५. आत्मानन्द से बढ़ कर और कोई आनन्द नहीं है।
२६. आत्मा से बढ़ कर और कोई मित्र नहीं है।
२७. कम खायें। गहरी श्वास लें। मधुर शब्द बोलें। उत्साहपूर्वक कार्य करें।
२८. वही सोचें जो कल्याणकारी है। अपने संकल्पों को ईमानदारी से पूरा करें। अपने कार्य के प्रति उत्साह रखें। उसे दृढ़ता से करें तथा उसे करने में ढिलाई न दिखायें। विनयशील बनें। पूरे मन से प्रार्थना करें।
२९. साहसपूर्वक धैर्य रखें। धैर्यपूर्वक सहन करें। पूरी सजगता के साथ मन को एकाग्र करें। उत्साहपूर्वक ध्यान करें। तब ईश्वर का साक्षात्कार करने में देर नहीं लगेगी।
३०. सर्वोच्च चेतना तथा ध्यान के परमानन्द के समक्ष ऐन्द्रिक सुख कुछ भी नहीं है।
३१. बुद्धि के द्वार बन्द करें। इन्द्रियों के झरोखे बन्द करें। हृदय के नीरव शान्त मन्दिर में अवस्थित हो कर उच्चतर चेतना की सहज निद्रा का आनन्द लें।
३२. इन्द्रियों और विचारों पर नियन्त्रण किये बिना आध्यात्मिक विकास सम्भव नहीं है।
३३. अपशब्द और आलोचना मात्र शब्दों के खेल या हवा के प्रदोलन (vibrations) हैं।
३४. प्रशंसा से प्रभावित न हों। परम सत्ता से तादात्म्य स्थापित करें।
३५. अधिकतम जीवन ऊर्जा और शान्ति की स्थिति में ध्यान करने से - अध्यात्म-शक्ति का पूर्ण विकास होता है।
३६. प्रार्थना, ध्यान, अहिंसा तथा संयम से मानव-स्वभाव परिशुद्ध होता है।
३७. ध्यान से आन्तरिक शक्ति, शुद्ध शान्ति, साक्षात्कार तथा परमानन्द प्राप्त होते हैं।
३८. प्रत्येक अवरोध से योग की सीढ़ी के अगले डण्डे पर पैर रखने की शक्ति प्राप्त होती है।
३९. अज्ञान से खिन्नता, उदासी तथा विनाश की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आत्मा का साक्षात्कार करें तथा सबके साथ सामंजस्य रखें।
४०. प्रत्येक अवरोध इच्छा-शक्ति को विकसित करने का एक अवसर है।
४१. कष्टों, दुःखों और संकटों में धैर्य रखें। हीरे की तरह कठोर बन कर अवरोधों को पराभूत करें।
४२. कामुकता से जीवन की कान्ति, व्यक्तित्व, जीवन-शक्ति, स्मृति, सामर्थ्य, पवित्रता, प्रतिष्ठा, शान्ति, ज्ञान और निष्ठा का विनाश हो जाता है; इसलिए काम-रूपी शत्रु का संहार करें।
४३. अनुभवहीन विद्यार्थी अपनी कल्पना तथा मनोवेगों को अपनी अन्तर्वाणी समझने की भूल कर बैठते हैं।
४४. अहं और कामुकता के त्याग में ही आत्म-त्याग का रहस्य छिपा हुआ है।
४५. संसार में रहें, परन्तु सांसारिक न बनें। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए सांसारिक प्रलोभनों के बीच पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वही सर्वोच्च साधक है।
४६. अपनी अज्ञानता से आप ईश्वर को भूल जायें, तो भी ईश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा।
४७. दुर्जनों की संगति में न रहें।
४८. आपके अन्दर ज्ञान और शक्ति के अपरिमेय तथा अक्षय स्रोत वाला कुआँ है। इस कुएँ के जल का उपयोग करें। अपनी गहराइयों में उतरें तथा अमरता के पवित्र जल में पैठें।
४९. जगत् के नियमों को समझें और उनके अनुकूल बनें।
५०. प्रत्येक अवरोध आपको अपनी बलवती इच्छा को विकसित करने तथा अपनी शक्ति में अभिवृद्धि करने का अवसर प्रदान करता है।
५१. अपना विकास करें, संवर्धन करें। हृदय की विशालता, सहज बुद्धि तथा साहस के रचनात्मक सद्गुणों (दैवी सम्पद) का विकास करें। अध्यात्म मार्ग पर चलें - और इस तथ्य को हृदयंगम करें—मैं ही अमर आत्मा हूँ।
५२. प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आचरण न करें।
५३. जो दुःखी हैं, उन्हें धैर्य बँधायें ।
५४. कूटनीति और मिथ्याचार से दूर रहें।
५५. भोग-विलास से दूर रहें।
५६. सबके साथ ऐक्य-भाव रखें।
५७. आध्यात्मिक विचारों से मन का उत्थान करें। ब्रह्म के गहन, एकाग्र चिन्तन द्वारा इसका विस्तार करें।
५८. प्रत्येक कार्य ईश्वर हेतु किया गया एक यह है। अनुभव करें कि प्रत्येक प्राणी उसकी ही प्रतिकृति (सृष्टि) है।
५९. ईश्वर को कण-कण में तथा प्रत्येक प्राणी में देखें।
६०. ईश्वर सर्वव्यापी है। वह भिखारियों के वेश में दीन बन कर रहता है। वह बीमार बन कर दुःखी होता है। वही जंगलों में चिथड़े-लत्ते लपेटे घूमता है। प्रत्येक प्राणी में उसे देखें। सबकी सेवा करें, सबको प्रेम करें।
६१. तीन बातें आवश्यक हैं— ईश्वर में विश्वास, प्रायश्चित्त और त्याग करने की तत्परता ।
६२. तीन बातें प्रशंसनीय हैं—सत्यता, ईमानदारी और हृदय की विशालता ।
६३. तीन बातों पर नियन्त्रण करें-जिह्वा, क्रोध और अशान्ति उत्पन्न करने वाले विचार |
६४. तीन बातें उपयोगी हैं—वैश्व-प्रेम, करुणा तथा धैर्य ।
६५. तीन बातें प्रीतिकर हैं—मोक्ष की कामना, सत्संग तथा निःस्वार्थ सेवा।
६६. तीन बातों से बचें—लोलुपता, क्रूरता तथा ओछापन ।
६७. तीन बातें त्याज्य हैं—कामुकता, दुर्जनों का संग तथा कर्म-फलाशा।
६८. तीन बातें एक ही पूर्ण इकाई के भाग हैं—सेवायोग, समर्पणयोग और ज्ञानयोग ।
६९. बाल-सुलभ व्यवहार करें, बचकाना व्यवहार नहीं।
७०. भक्ति भावना अपेक्षित है, भावुकता नहीं।
७१. दृढ़ इच्छा शक्ति रखें। हठधर्मिता अपेक्षित नहीं है।
७२. किसी एक आदर्श पर दृढ़ रहें। असहिष्णु न बनें।
७३. साहसी बनें; लेकिन जान-बूझ कर खतरे मोल न लें।
७४. स्पष्टवादी बनें; परन्तु छिद्रान्वेषण न करें।
७५. भद्र बनें, साथ ही साथ निर्भीक भी सादगी रखें; परन्तु आत्म गौरव को न भूलें।
७६. किसी दोष से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है, उसके विरोधी गुण का खूब मनन करना तथा उस गुण को व्यवहार में लाना।
७७. सेवा धर्म है। सेवा करें। प्रेम करें। दूसरों को खूब 'दें'। अपने को पवित्र करें।
७८. भले बनें। भलाई करें। दयालु बनें। पवित्र बनें।
७९. दूसरों की सुनें, उस पर चिन्तन करें; ध्यान का अभ्यास करें और परम तत्त्व का साक्षात्कार करें।
८०. ईश्वर की कृपा पर सदैव आस्था रखें। उससे बालक की तरह बोलें। उसके सामने अपना हृदय खोल कर रख दें। उसकी कृपा की वर्षा आपके ऊपर तुरन्त होगी।
८१. व्यर्थ बातें न करें।
८२. मधुर शब्द किसी को भी हानि नहीं पहुँचाते हैं। हाँ, हृदय की निष्ठुरता के वे शत्रु हैं।
८३. पूरे संसार में एक ही जाति है— मानव-जाति
८४. पहले ध्यान और अनुशासन की सहायता से अपने अन्दर शान्ति प्राप्त करें;
तब दूसरों को शान्ति प्रदान करने का प्रयत्न करें।
८५. दूसरों के अनुकूल बनें; सद्भावपूर्ण बनें, नमनशील बनें। अपमान और क्षति को सहन करें।
८६. जो आपको हानि पहुँचाये या सताये, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें।
८७. जो आपकी निन्दा करे, उसकी सेवा करें।
८८. जो आपके साथ अन्याय करे, उसको प्रेम करें।
८९. जो हृदय को शुद्ध करे, वह सद्गुण है; जो हृदय को दूषित करे, वह पाप है।
९०. जो आपको ईश्वर के निकट लाये, वह सद्गुण है; जो आपको अज्ञान के गर्त में गिरा दे, वह पाप है।
९१. जो आपको शान्ति, प्रसन्नता, सन्तोष और प्रफुल्लता प्रदान करे तथा आपके हृदय को विशाल बनाये, वह सद्गुण है। जिससे आपको अशान्ति उदासी और अवसाद मिले, वह पाप है।
९२. कामुकता अतोषणीय है। यह दुःख, पीड़ा, विपत्ति और अप्रसन्नता का स्रोत है।
९३. ईर्ष्या रखना तुच्छता है। स्वार्थी होना लज्जा की बात है। दयालुता दैवी गुण है। धैर्य और सहनशीलता पौरुष की निशानी हैं। कामुकता से मुक्त होने से लाभ ही लाभ है। शान्त और तनाव रहित होना प्रशंसनीय है।
९४. बुरे विचार बुरे कार्यों की ही तरह बुरे होते हैं।
९५. ईश्वर के साथ सजगतापूर्वक सम्पर्क करके उच्चतर सत्य की प्राप्ति की जाती है। वस्तुतः यही योग है।
९६. ऐन्द्रिय सुखों के पीछे जितना ही आप भागेंगे, उतना ही आप अशान्त और उत्तेजित होंगे।
९७. अपने अस्तित्व के सभी भागों के प्रति पूर्ण रूप से सजग हो जायें। सदैव जागरूक और व्यस्त रहें। आपकी उपस्थिति आपके शब्दों से अधिक अभिव्यक्तिशील होनी चाहिए।
९८. आध्यात्मिक अभ्यास से आपके आन्तरिक जीवन की सम्पदा बढ़नी चाहिए; आपको वस्तुओं के आध्यात्मिक मूल्यों का बोध प्राप्त होना चाहिए और प्रत्येक परिस्थिति में शान्त बने रहने की क्षमता मिलनी चाहिए।
९९. आपके हृदय में करुणा हो, हाथों में उदारता हो, शब्दों में मधुरता हो, विचारों में सन्तुलन हो, मन दुराग्रहों से मुक्त हो; आप सेवाभावी बनें।
१००. आप कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर सदैव आपके हृदय में है, आपके साथ है। यह आपके अत्यन्त निकट है। जितनी आपको उसकी आवश्यकता है, उससे अधिक उसे आपकी आवश्यकता है; अतः समस्त आतंकों और भयों से मुक्त हो जायें।