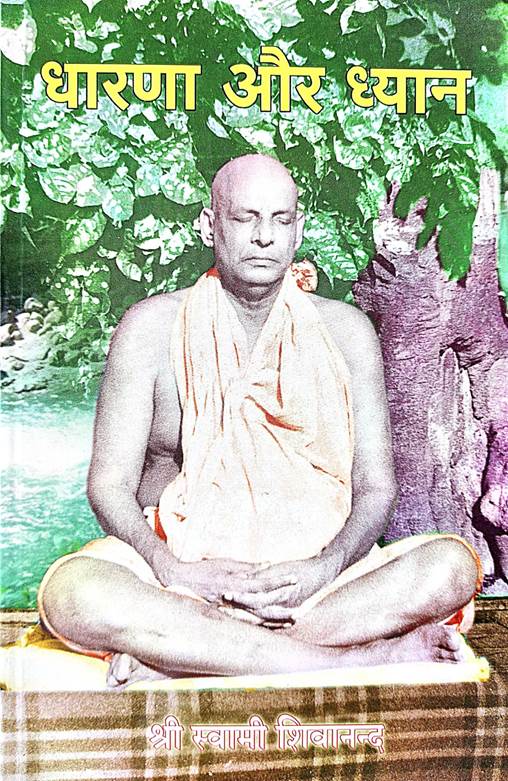
धारणा और ध्यान
CONCENTRATION AND MEDITATION
का हिन्दी अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती
MEDITATE REALIZE LOVE
THE DIVINE LIFE SOCIETY
अनुवादिका
शिवानन्द राधिका अशोक
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय शिवानन्दनगर – २४९१९२
जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.disha.org
प्रथम हिन्दी संस्करण: २००८
द्वितीय हिन्दी संस्करण : २०११
तृतीय हिन्दी संस्करण २०१५
चतुर्थ हिन्दी संस्करण : २०२१
(१,००० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
HS 7
PRICE : ₹210/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा
प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी प्रेस,
पो. शिवानन्दनगर – २४९ १९२, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित ।
For online orders and Catalogue visit: disbooks.org
---------------------------------------------
ॐ
उन योगियों तथा भक्तों
को
समर्पित
जो धारणा तथा ध्यान द्वारा
जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है ।
---------------------------------------------
परिचय
धारणा एवं ध्यान सिद्धि हेतु राज मार्ग है। धारणा ध्यान हेतु प्रेरित करती है। मन को शरीर के बाहर अथवा भीतर किसी एक बिन्दु पर केन्द्रित करके, उसे वहाँ कुछ देर के लिए स्थिर कीजिए। यह धारणा है। आपको इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। पहले उत्तम आचरण के अभ्यास द्वारा अपने मन को स्थिर कीजिए, तत्पश्चात् धारणा का अभ्यास कीजिए। मन की शुद्धता के बिना धारणा का कोई लाभ नहीं है। कुछ तान्त्रिक ऐसे हैं जिनकी धारणा तो होती है, लेकिन उनका चरित्र अच्छा नहीं होता। यही कारण है कि वे आध्यात्मिक मार्ग में किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर पाते।
वह जिसका आसन स्थिर है तथा जिसने प्राणायाम के निरन्तर अभ्यास द्वारा अपनी नाड़ियों तथा कोशों को शुद्ध कर लिया है, वह अच्छी धारणा कर सकता है।
यदि आप सभी विचलनों को दूर हटा दें, तो धारणा तीव्र होगी। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिसने अपनी शक्ति का संरक्षण किया है, उसकी धारणा अपूर्व होगी।
कुछ मूर्ख अधैर्यवान् साधक बिना किसी प्रारम्भिक नैतिक प्रशिक्षण के एकदम धारणा करने लग जाते हैं। यह भयंकर भूल है। नैतिक पूर्णता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।
आप आध्यात्मिक ऊर्जा के सातों चक्रों में से किसी एक पर आन्तरिक रूप से धारणा कर सकते हैं। अवधान धारणा में प्रमुख भूमिका निभाता है। जिसने अपनी अवधान की शक्ति का विकास कर लिया है, उसकी धारणा अच्छी होती है। वह मनुष्य जो वासना तथा सभी प्रकार की काल्पनिक कामनाओं से पूर्ण है, वह किसी भी वस्तु अथवा विषय पर कठिनाई से एक सेकेंड तक ही धारणा कर सकेगा। उसका मन बूढ़े बन्दर की भाँति इधर से उधर कूदता रहता है।
एक वैज्ञानिक अपने मन को एकाग्र करता है तथा कई नये आविष्कार करता है। धारणा के द्वारा वह अपने स्थूल मन की पर्तें खोलता है और मन के उच्च लोकों में गहरे उतर जाता है तथा गहन ज्ञान प्राप्त करता है। वह अपने मन की समस्त शक्तियों को एक जगह केन्द्रित करके उन्हें उन पदार्थों पर फेंकता है, जिनका वह विश्लेषण कर रहा है तथा उनके रहस्यों को खोज लेता है।
वह जिसे प्रत्याहार (इन्द्रियों को विषयों से वापस खींचना) का ज्ञान है, उसकी अच्छी धारणा होती है। आध्यात्मिक मार्ग में आपको शनैः-शनैः एक-एक कदम आगे बढ़ना होगा। धारणा का अभ्यास प्रारम्भ करने के लिए अच्छे आचरण, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार की नींव रखिए। धारणा एवं ध्यान का भवन तभी सफलतापूर्वक खड़ा होगा।
आपको धारणा के विषय को उसकी अनुपस्थिति में भी स्पष्ट रूप से देख सकते योग्य होना चाहिए। एक क्षण में ही उसका मानसिक चित्र आपकी आँखों के सामने आ जाना चाहिए। यदि आपकी धारणा अच्छी होगी, तो आप ऐसा बिना किसी कठिनाई के कर सकेंगे।
प्रारम्भ में आप घड़ी की टिकटिक, मोमबत्ती की ली अथवा अन्य किसी विषय पर, जो आपके मन को अच्छा लगे, धारणा का अभ्यास कर सकते हैं। मन के अवलम्बन के लिए किसी विषय के बिना धारणा सम्भव नहीं है। कोई भी विषय, जो मन को रुचिकर लगे, उस पर मन को स्थिर किया जा सकता है। प्रारम्भ में मन को जो नापसन्द हो, ऐसे विषय पर उसे एकाग्र करना बड़ा ही कठिन है।
जो धारणा का अभ्यास करते हैं, वे शीघ्र उन्नति करते हैं। वे किसी भी कार्य को वैज्ञानिक ढंग से, बिना किसी गलती के तथा पूर्ण दक्षता से कर सकते है। जिस कार्य को अन्य छह घण्टों में करते हैं, उसे धारणा का अभ्यासी आधे घण्टे में कर सकता है। धारणा उमड़ते हुए आवेगों को शान्त करती है, शुद्ध करती है। यह विचार शक्ति को दृढ करती है तथा विचारों को स्पष्ट करती है। यह मनुष्य की भौतिक प्रगति में सहायता करती है। धारणा करने वाला अपने कार्य एवं व्यापार को अच्छे ढंग से सम्पन्न करता है। जो पहले धुंधला तथा अनिश्चित था, वह धारणा के अभ्यास से स्पष्ट और सुनिश्चित हो जाता है। जो पहले कठिन था, वह अब सरल हो जाता है और जो जटिल तथा भ्रमित करने वाला था, वह सरल एवं मन की पकड़ में हो जाता है। आप धारणा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो नियमित धारणा करते हैं, उनके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। यदि कोई भूखा अथवा किसी जटिल रोग से ग्रसित हो, तो उसके लिए धारणा करना कठिन है। धारणा का अभ्यास करने वाले की मानसिक दृष्टि एकदम स्पष्ट होती है।
मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान ही एकमात्र श्रेष्ठ मार्ग है। ध्यान सभी दर्दों, कष्टों, त्रिताप तथा पंच क्लेशों को नष्ट कर देता है। ध्यान समदृष्टि प्रदान करता है। ध्यान एक हवाई जहाज के समान है, जो परमानन्द एवं स्थायी शान्ति के धाम की ओर बढ़ने में सहायक होता है। यह एक अद्भुत सीढ़ी है, जो पृथ्वी और स्वर्गलोक को जोड़ती है। तथा साधक को ब्रह्म के अमर धाम को ले कर जाती है।
ध्यान ईश्वर अथवा आत्मा के एक ही विचार का तैलधारावत् प्रवाह है। ध्यान धारणा का अनुगामी होता है।
प्रातः काल ब्राह्ममुहूर्त में ४ से ६ बजे तक ध्यान का अभ्यास करें। यह ध्यान हेतु सर्वश्रेष्ठ समय है।
पद्मासन अथवा सुखासन में बैठे सिर, गर्दन और धड़ एकसीध में होने चाहिए। त्रिकुटी, भूमध्य-स्थान अथवा हृदय पर ध्यान करें। नेत्रों को बन्द रखें।
ध्यान दो प्रकार का होता है—सगुण और निर्गुण। सगुण ध्यान में योगाभ्यासी भगवान् कृष्ण, राम, सीता, विष्णु, शिव, गायत्री अथवा देवी के रूप का ध्यान करता है। निर्गुण ध्यान में वह अपनी आत्मा पर ध्यान करता है।
चतुर्भुज भगवान् हरि के चित्र को अपने सामने रखिए। पाँच मिनट तक इसे स्थिर दृष्टि से देखें, तत्पश्चात् नेत्र बन्द कर लें और चित्र को नेत्रों को बन्द किये हुए ही देखने का प्रयास करें। मन को भगवान् के अंगों पर ले कर जायें। मानसिक रूप से पहले उनके चरणों को देखिए; फिर पैरों को, उसके बाद पीताम्बर को, तत्पश्चात् वक्षस्थल के कौस्तुभ मणि जड़ित स्वर्ण हार को देखें, उसके बाद उनके मकराकृति कुण्डलों को, फिर मुख मण्डल को, उसके बाद मुकुट को, उसके बाद दायें हाथ में चक्र को, उसके बाद बायें हाथ में कमल को, फिर पैरों को, उसके बाद ऊपरी बायें हाथ में शंख को, तत्पश्चात् निचले बायें हाथ में गदा को देखें। इसके बाद पूरी विधि को पुनः दोहरायें । मन में 'हरि ॐ' अथवा 'ॐ नमो नारायणाय' का जप करें। भगवान् के सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, पवित्रता आदि गुणों के बारे में चिन्तन करें।
ॐ तथा इसके अर्थ का भाव सहित ध्यान करें। यह निर्गुण ध्यान है। मानसिक रूप से ॐ का जप करें। स्वयं को आत्मा के साथ जोड़ें। अनुभव करें— “मैं सर्वव्यापक आत्मा हूँ। मैं सत्-चित्-आनन्द ब्रह्म हूँ। मैं तीनों कालों का तथा मन के सभी रूपान्तरों का मौन साक्षी हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। मैं शरीर, मन, प्राण तथा इन्द्रियों से पृथक् हूँ। मैं स्वप्रकाश्य ज्योतिस्वरूप हूँ। मैं अमर परम आत्मा हूँ।”
यदि आपमें सन्तोष, उत्साह, धैर्य, मन की अविचल स्थिति, मधुर वाणी, मन की एकाग्रता, हल्का शरीर, निर्भयता, निष्काम्यता, सांसारिक वस्तुओं के प्रति अरुचि है, तो जानें कि आप आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर रहे हैं तथा आप ईश्वर के सन्निकट हैं।
हे प्रेम! एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको किसी प्रकार की ध्वनि नहीं सुनायी देगी, न आपको कोई रंग दिखायी देगा। वह स्थान है परम धाम या परम अनामय स्थान (दर्द रहित स्थान)। यह शान्ति और आनन्द का अमर धाम है। यहाँ शारीरिक चेतना नहीं रहती। यहाँ मन विश्राम प्राप्त करता है। सभी कामनाएँ तथा तीव्र अभिलाषाएँ जाती है। यहाँ इन्द्रियाँ शान्त रहती है, बुद्धि कार्य करना बन्द कर देती है। यहाँ कोई नहीं होता। क्या आप गहन ध्यान द्वारा इस शान्ति स्थल की खोज करेंगे? यहाँ परम शान्ति का साम्राज्य है। प्राचीन काल में ऋषियों ने एकान्त में मन को विलीन करके ही इस स्थान को प्राप्त किया था। यहाँ ब्रह्म स्वप्रकाश्य ज्योति में ज्योतित होता है।
शरीर को भूल जायें। अपने आस-पास सभी कुछ भूल जायें। भूलना सबसे बड़ी साधना है। यह ध्यान में बड़ी सहायक है। इसके द्वारा भगवान् के निकट पहुँचने में सरलता होती है। ईश्वर को स्मरण करने से आप सब कुछ भूल सकेंगे। मन को विषय-वस्तुओं से वापस खींच कर और इसे अपनी हृदय गुहा में प्रकाशित हो रहे ईश्वर के चरणों में लगा कर आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करें। गहन शान्त ध्यान के अभ्यास द्वारा अपने भीतर गहरे उतर कर लीन हो जायें। गहरे गोते लगायें। सत्-चित्-आनन्द के सागर में उन्मुक्तता से तैरें। आनन्द की दिव्य सरिता में हैं। स्रोत का दोहन करें। देवी चेतना के स्रोत की ओर सीधे आगे बढ़ें और अमृत पान करें। दैवी आलिंगन को अनुभव करें और दैवी समाधि का आनन्द लें। अब यहाँ मैं आपको छोड़ दूंगा। अब आपने अमरत्व एवं निर्भयता की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। हे प्रेम! भयभीत न हों, देदीप्यमान हों, उनका प्रकाश आ गया है।
जितना अधिक आप ध्यान करेंगे, उतना ही अधिक आपको वह आन्तरिक जीवन प्राप्त होगा, जहाँ मन तथा इन्द्रियाँ कार्य नहीं करती है।
आप मूल स्रोत आत्मा के अत्यन्त निकट होंगे। आप आनन्द एवं शान्ति की लहरों का आनन्द लेंगे।
समस्त विषय-वस्तुओं के प्रति आपको कोई आकर्षण नहीं रहेगा। यह जगत् आपके सामने दीर्घ स्वप्न जैसा दृष्टिगोचर होगा। निरन्तर गहन ध्यान द्वारा आपके भीतर ज्ञान का सुप्रभात होगा।
आप पूर्ण ज्ञानी हो जायेंगे। अब अज्ञानता का आवरण नष्ट हो गया है। आपके समस्त कोशों का भेदन हो गया है। आपके भीतर से देहाध्यास नष्ट हो जायेगा। आप 'तत् त्वं असि' महावाक्य के महत्त्व को पहचान लेंगे। सभी भेद, उपाधियाँ तथा गुण अदृश्य हो जायेंगे। आप सर्वत्र आनन्द, प्रकाश तथा ज्ञान से पूर्ण अनन्त आत्मा के दर्शन करेंगे। यह वास्तव में एक दुर्लभ अनुभव होगा। अर्जुन की भाँति भय से न करें। यहाँ पर इन्द्रियाँ नहीं है। यहाँ शुद्ध चेतना मात्र है।
हे प्रेम! आप आत्मा हैं। आप यह नश्वर शरीर नहीं है। इस घृणित शरीर के प्रति मोह त्याग दें। भविष्य में कभी भी यह न कहे "मेरा शरीर" कहें- "यह उपकरण" अब सूर्यास्त होने को है, सूर्य अपनी सभी किरणों को भीतर समेट रहा है। अब ध्यान हेतु बैठ जायें। अपने भीतर की त्रिवेणी में गहरे गोते लगायें। मन की सभी किरणों को एकत्र करें और आन्तरिक हृदय गुहा में गहरे लीन हो जायें। सभी प्रकार के भय, उत्तरदायित्वों, चिन्ताओं, आकुलताओं को त्याग दें। एकान्त के सागर में विश्राम करें । अनन्त शान्ति का आनन्द लें। आपका पुराना शरीर अब चला गया है। सभी सीमाएँ अदृश्य हो गयी हैं। यदि कामनाएँ और पुरानी अभिलाषाएँ पुनः फुफकारने का प्रयत्न करें, तो उन्हें विवेक की लाठी और वैराग्य की तलवार से नष्ट कर दें।
जब तक आप ब्रह्म-स्थिति को न प्राप्त कर लें, इन दोनों को सदा अपने पास रखें। ॐ सत् चित् आनन्द है। ॐ अनन्त है। ॐ का ध्यान करें।
ॐ ॐ ॐ की गर्जना करें। ॐ ही सुनें। ॐ का स्वाद लें। ॐ का दर्शन करें। ॐ का पान करें। ॐ आपका नाम है। यही ॐ आपका नाम है। यही ॐ आपका पथ-प्रदर्शन करे! ॐ ॐ ॐ ॐ शान्तिः।
-स्वामी शिवानन्द
ध्यानश्लोकम्
ॐ
॥ शिवध्यानम् ॥
शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं
शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणांगे वहन्तम् ।
नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितां चांकुशं वामभागे
नानालंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥
मैं पंचमुखी श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ जो पार्वती जी के स्वामी हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषण धारण किये हैं, जो स्फटिक मणि के समान दीप्तिमान हैं, जो पद्मासन में स्थित हैं, चन्द्रमा जिनका मुकुट है, जिनके तीन नेत्र हैं, जो दाहिनी ओर त्रिशूल, वज्र, खड्ग एवं बार्थी ओर नागपाश, घण्टा, डमरु तथा अंकुश धारण किये हैं। जो अपने भक्तों की सभी भयों से रक्षा करते हैं।
ॐ
।। शंकराचार्यध्यानम् ।।
पद्मासीनं प्रशान्तं यमनिरतमनंगारितुल्यप्रभावं
फाले भस्मांकिताभं स्मितरुचिरमुखांभोजमिन्दीवराक्षम्म् ।
कम्बुग्रीवं कराभ्यामविहतविलसत्पुस्तकं ज्ञानमुद्रां
वन्दयै गीर्वाणमुख्यैर्नतजनवरदं भावये शंकरार्यम् ।
मैं श्री शंकराचार्य जी का ध्यान करता हूँ, जो पद्मासन में ज्ञानमुद्रा में बैठे हैं, जो शान्त हैं, जो यम-नियम आदि सद्गुणों से युक्त हैं, जिनकी कीर्ति भगवान् शंकर के समान है, जिनके मस्तक पर भस्म अंकित है, जिनका मुख खिले कमल के समान है, जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान हैं, जो हाथों में वेद लिये हुए हैं, जिनकी आराधना महत् बुद्धि सम्पन्न जन करते हैं तथा जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं।
ॐ
॥ ओंकारध्यानम् ॥
ओंकारं निगमैकवेद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं
चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकम् ।
विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः सम्प्रोच्यमानं विभुं
सत्यज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे ॥
मैं नित्य-शुद्ध, सर्वव्यापक, प्रणव, ओंकार का सदैव ध्यान करता हूँ, जिसे विभिन्न श्रुतियों में वेदान्त का स्रोत एवं आधार कहा गया है, जिसे इस विश्व की सृष्टि, अस्तित्व तथा विलय का कारण कहा जाता है, जो इस विश्व की आत्मा है तथा जो सत्य, ज्ञान और अनन्तता है।
ॐ
।। दत्तात्रेयध्यानम् ।।
मालाकमण्डलुधरः करपद्मयुग्मे
मध्यस्थपाणियुगले डमरुत्रिशूलम् ।
अध्यस्थ ऊर्ध्वकरयोः शुभशंखचक्रे
वन्दे तमत्रितनयं भुजषट्कयुक्तम् ॥
मैं अत्रि-पुत्र दत्तात्रेय का ध्यान करता हूँ, जिनके छह हाथ हैं, जिनके नीचे के दोनों हाथों में माला और कमण्डल, मध्य के दोनों हाथों में डमरु और त्रिशूल तथा ऊपरी दोनों हाथों में शंख और चक्र हैं।
ॐ
॥ गणेशध्यानम् ॥
गजाननं भूतगणादिसेवितं
कपित्थजम्बूफलसारभक्षणम् ।
उमासुतं शोकविनाशकारणं
नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम् ॥
मैं उमा-पुत्र श्री गणेश के चरण-कमलों में नमन करता हूँ, जो सभी दुःखों का नाश करते हैं, भूत गण तथा देव जिनकी सेवा करते हैं तथा जो जम्बू और कपित्थ फल के सार को ग्रहण करते हैं।
ॐ
॥ सुब्रह्मण्यध्यानम्॥
षडाननं कुंकुमरक्तवर्णं
महामतिं दिव्यमयूरवाहनम् ।
रुद्रस्य सुनूं सुरसैन्यनाथं
गुहं सदाहं शरणं प्रपद्ये ॥
मैं षडानन भगवान् गुह के चरणों का सदा ध्यान करता हूँ, जो कुंकुम के समान रक्त वर्ण के तथा जो अनन्त ज्ञान हैं, जिनका वाहन दिव्य मयूर है, जो देवों की सेना के नायक हैं।
ॐ
।। सरस्वतीध्यानम् ।।
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ।।
वे देवी सरस्वती मेरी रक्षा करें जो शुभ्र वर्ण की हैं, हिम के समान श्वेत कुन्दों के पुष्पों को धारण करती हैं, शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, श्रेष्ठ पवित्र वीणा लिये हुए श्वेत कमल पर विराजित हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जिनकी आराधना करते हैं तथा जो जड़ता और आलस्य को दूर करने वाली हैं।
ॐ
॥ महालक्ष्मीध्यानम् ।
वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां
हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषिताम् ।
भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिस्सेवितां
पार्श्वे पंकजशंखपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः ॥
मैं श्री लक्ष्मी देवी का ध्यान करता हूँ, जो हाथों में कमल लिये हैं, प्रसन्न मुख हैं, सौभाग्य को देने वाली हैं, जो दोनों हाथों से अभय प्रदान करती हैं, जो अनेक मणियों से सुशोभित हैं, जो अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करती हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जिनकी आराधना करते हैं, शक्तियाँ जिनके आस-पास रहती हैं और जो शंख, पद्म तथा महापद्मा निधि से युक्त हैं।
ॐ
॥ कृष्णध्यानम् ॥
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् ।
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ।।
मैं कमलनयन वंशीधर कृष्ण, जो काले मेघ के समान वर्ण वाले हैं, जिनके ऑट लाल बिम्ब फल की भाँति हैं, जिनका मुख पूर्ण चन्द्र की भाँति प्रकाशित हो रहा है, के. सिवा अन्य किसी को नहीं जानता।
ॐ
॥ रामध्यानम् ।।
ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं
पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् ।
वामांकारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं
नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् ।
श्री रामचन्द्र जी का ध्यान करो, जो आजानुबाहु हैं, जो पद्मासन में बैठे हैं, पोत वस्त्र धारण किये हैं, जिनके नेत्र नव-प्रस्फुटित कमल की पंखुड़ी की भाँति हैं, जिनकी चाल अत्यन्त सुन्दर है, जिनकी बायीं ओर सीता जी विराजमान हैं, जिनका वर्ण मेघ के समान श्याम है, जिन्होंने अनेक आभूषण धारण किये हैं तथा जिनके शीश पर विशाल जटा सुशोभित है।
ॐ
॥ गायत्रीध्यानम् ॥
मुक्ताविद्रुमहेमनीलधवलच्छायैर्मुखैस्तीक्षणै-
युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम् ।
गायत्री वरदाभयांकुशकशां शुभ्रं कपालं गदां
शंखं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ॥
मैं श्री गायत्री माता का ध्यान करता हूँ, जिनका मुख मोतियों, मूँगे, स्वर्ण, नीले एवं श्वेत रत्नों से सुशोभित है, जिनका मुकुट मोतियों और चन्द्रमा से अलंकृत है, जो सभी वेदों के सार को व्यक्त करती हैं, जो उस पवित्र सत्य की मूर्ति हैं, जो अपने दोनों हाथों से वरदान तथा अभय प्रदान करती है तथा जो अपने हाथों में अंकुश, चाबुक, खप्पर, गदा, शंख, चक्र तथा दो श्वेत कमल लिये हैं।
ॐ
॥ सूर्यध्यानम् ॥
भास्वद्रत्नाढ्यमौलिः स्फुरदधररुचा रंजितश्चारुकेशो
भास्वान्यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः स्वर्णवर्णः प्रभाभिः ।
विश्वाकाशावकाशग्रहपतिशिखरे भाति यश्चोदयाद्रौ
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षुः ॥
जो जगत् के नेत्र हैं, जो समस्त आनन्द के दाता हैं, जो भगवान् हरि, शिव एवं देवों द्वारा पूजित हैं, जो ऊँचे पहाड़ों में चमकते हैं, जो रत्न जड़ित मुकुट के साथ देदीप्यमान हैं, जो ग्रहों के देव हैं, जिन्होंने इस सम्पूर्ण जगत् को व्याप्त किया है, जो अपने ओठों तथा सुन्दर केशों की दीप्ति के साथ प्रकाशित हैं तथा दिव्य तेज से युक्त हैं, वे सूर्यदेव मेरी रक्षा करें।
विषय-सूची
४. अन्तर्मुख एवं बहिर्मुख वृत्तियाँ
६. मन की घुमन्तु प्रवृत्ति को कम करें
३. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धारणा
४. ब्राह्ममुहूर्त - -ध्यान हेतु सर्वश्रेष्ठ समय
१३. ध्यानाभ्यास के लिए योग्यताएँ
३. नेत्र बन्द कर मानसिक चित्रण करना
६. सगुण तथा निर्गुण ध्यान की तुलना
११. पुराने कुसंस्कारों का दबाव
२५. पूर्वाग्रह, असहिष्णुता और हठधर्मिता
बीस महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक नियम
धारणा और ध्यान
अध्याय १
धारणा का सिद्धान्त
१. धारणा क्या है?
"देशबन्धश्चित धारणा "मन को किसी बाह्य विषय अथवा आन्तरिक बिन्दु पर एकाग्र करना धारणा है। एक बार एक संस्कृत के विद्वान कबीर के पास गये और उनसे प्रश्न किया "कबीर, अभी आप क्या कर रहे हैं?" कबीर ने उत्तर दिया पण्डित जी, मैं मन को सांसारिक विषयों से वापस खींच कर भगवान् के चरण कमलों पर एकाग्र कर रहा हूँ।" इसे धारणा कहते हैं। उत्तम आचरण, आसन-प्राणायाम तथा विषय-वस्तुओं से प्रत्याहार धारणा में शीघ्र सफलता प्राप्ति को सरल बनाते हैं। धारणा योग की सीढ़ी का छठवाँ पायदान है। मन जिस पर टिक सके, ऐसी किसी वस्तु के बिना धारणा नहीं हो सकती। एक निश्चित उद्देश्य, रुचि, एकाग्रता धारणा में सफलता लाते हैं।
इन्द्रियाँ आपको बाहर खींच लाती है और आपके मन की शान्ति को भंग कर देती हैं। यदि आपका मन बैचैन है, तो आप किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते हैं। जब अभ्यास के द्वारा मन की किरणें एकत्रित हो जाती हैं, तो मन एकाग्र हो जाता है और आपको मन के भीतर से आनन्द प्राप्त होता है। विचारों और आवेगों को शान्त करें।
आपके भीतर धैर्य, दृढ़ संकल्प तथा अथक दृढ़ता होनी चाहिए। आपको अपने अभ्यास में बड़ा ही नियमित होना चाहिए, अन्यथा आलस्य और विपरीत बल आपको लक्ष्य से दूर ले के चले जायेंगे। एक उत्तम प्रशिक्षित मन को संकल्प के अनुसार किसी भी विषय पर, चाहे वह बाहरी हो या आन्तरिक, सभी विचारों के निषेध के लिए एकाग्र किया जा सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ विषयों पर धारणा हेतु क्षमता होती है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए धारणा का अत्यन्त उच्च स्तर तक विकास हो जाना चाहिए। उत्तम धारणा वाले व्यक्ति की अर्जन क्षमता अच्छी होती है तथा वह कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। धारणा करते समय मस्तिष्क पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। आपको मन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए।
एक पुरुष जिसका मन वासनाओं तथा विभिन्न प्रकार की काल्पनिक कामनाओ से पूर्ण है, वह मन को किसी विषय पर एक पल के लिए भी कठिनाई से ही एकाग्र कर सकेगा। ब्रह्मचर्य का पालन, प्राणायाम के अभ्यास, आवश्यकताओं तथा गतिविधियों में कमी, विषय-वस्तुओं का त्याग, एकान्त का सेवन, मौनव्रत, इन्द्रियों पर संयम करने तथा कामवासना, लोभ, क्रोध का उन्मूलन करना, अनावश्यक लोगों से मिलने-जुलने से बचना, समाचारपत्र- पठन और सिनेमा देखने का त्याग उपर्युक्त बताये गये नियमों के पालन से धारणा-शक्ति में वृद्धि होती है।
संसार के कष्टों, दुःखों से मुक्ति के लिए एकमात्र मार्ग धारणा है। इसके अभ्यासी का स्वास्थ्य उत्तम तथा उसे मानसिक दृष्टि से उत्साहित रहना चाहिए। धारणा का अभ्यासी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। वह किसी भी कार्य को बड़ी कुशलता से सम्पन्न कर सकता है। धारणा आवेगों को शान्त करती है। विचार-शक्ति को दृढ़ बनाइए और विचारों को स्पष्ट कीजिए। यम तथा नियम के द्वारा मन को शुद्ध कीजिए। शुद्धता के बिना धारणा का कोई उपयोग नहीं है।
किसी मन्त्र का जप तथा प्राणायाम मन को स्थिर करेगा। विक्षेपों का उन्मूलन कीजिए और धारणा-शक्ति में वृद्धि कीजिए। धारणा तभी की जा सकती है, जब मन सभी प्रकार के विक्षेपों से मुक्त हो। किसी भी उस विषय पर जिसे मन पसन्द करता हो या जो आपको अच्छा लगे, उस पर धारणा करें। प्रारम्भ में मन को स्थूल विषयों पर धारणा द्वारा प्रशिक्षित करना चाहिए और बाद में आप सूक्ष्म विषयों तथा निर्गुण विचारों पर सफलतापूर्वक धारणा कर सकेंगे। अभ्यास में नियमितता सर्वाधिक आवश्यक है।
स्थूल रूप : दीवार पर एक काला बिन्दु, मोमबत्ती की लौ, चमकता हुआ तारा, चन्द्रमा ॐ का चित्र, भगवान् शिव, राम, कृष्ण, देवी अथवा अपने इश्देवता के चित्र को अपने सामने रख कर खुली आँखों से ध्यान करें।
सूक्ष्म रूप: अपने इष्टदेवता के चित्र के सामने बैठ जायें और आँखें बन्द कर लें। अपने इह्देवता का मानसिक चित्र अपनी दोनों भौहों के मध्य अथवा अपने हृदय में रखें। मूलाधार, अनाहत, आज्ञा अथवा अन्य किसी आन्तरिक चक्र पर धारणा करें। दैवी गुणों जैसे प्रेम, करुणा अथवा अन्य किसी निर्गुण विचार पर धारणा करें।
२. धारणा कहाँ करें?
हृदय-कमल (अनाहत चक्र) अथवा भूमध्य अथवा त्रिकुटी (दोनों भौहों के मध्य स्थान) अथवा नासिकाग्र पर धारणा करें। नेत्रों को बन्द रखें।
मन का स्थान आज्ञा चक्र है। यदि आप त्रिकुटी पर धारणा करेंगे, तो मन सरलता से एकाग्र हो जायेगा।
भक्तों को हृदय पर धारणा करनी चाहिए योगियों तथा वेदान्तियों को आज्ञा चक्र पर धारणा करनी चाहिए।
मन का अन्य स्थान है सहस्रार ( सिर का शीर्ष स्थान)। कुछ वेदान्ती यहाँ पर धारणा करते हैं। कुछ योगी नासिकाग्र पर भी धारणा करते हैं (नासिकाग्र दृष्टि)।
धारणा के एक केन्द्र पर दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते रहें। इसे हठपूर्वक पकड़े रहें। यदि आप हृदय पर धारणा करते हैं, तो सदा इसी पर करते रहें, इसे कभी न बदलें। यदि आप आस्थावान् है, तो आपके गुरु धारणा हेतु केन्द्र का चुनाव करेंगे। यदि आप आत्म-निर्भर व्यक्ति हैं, तो आप स्वयं ही केन्द्र का चुनाव कर सकते हैं।
भ्रूमध्य-दृष्टि अर्थात् दोनों भौंहों के मध्य दृष्टि को केन्द्रित करना। यह आज्ञा चक्र का क्षेत्र है। अपने ध्यान के कमरे में पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ कर एक मिनट तक धारणा करें। इस समय को शनैः-शनैः आधा घण्टे तक बढ़ायें। इसमें बल-प्रयोग न करें। यह योग की क्रिया विक्षेप अथवा मन के भटकाव को रोकती है तथा धारणा का विकास करती है। भगवान् श्री कृष्ण ने गीता के पाँचवें अध्याय के २७ वें श्लोक में इस क्रिया-विधि को निर्दिष्ट किया है: “स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे ध्रुवो: "बाह्य सम्पर्कों को दूर करके दृष्टि को भ्रूमध्य में केन्द्रित करें। इसे भ्रूमध्य-दृष्टि भी कहते हैं; क्योंकि नेत्र भ्रूमध्य की ओर केन्द्रित किये जाते हैं। आप इसके सिवा नासिकाग्र दृष्टि का भी चुनाव कर सकते हैं। -
नासिकाग्र दृष्टि में दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर केन्द्रित करते हैं। जब आप सड़क पर भ्रमण कर रहे हों, तब भी नासिकाग्र दृष्टि रखें। भगवान् कृष्ण ने गीता के छठवें अध्याय के श्लोक १३ में इसका वर्णन इस प्रकार किया है "सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रम्” – चारों तरफ न देखते हुए, मात्र नासिका के अग्रभाग पर एकटक स्थिर दृष्टि से देखें यह अभ्यास मन को स्थिर करता है तथा धारणा-शक्ति का विकास करता है।
एक राजयोगी त्रिकुटी पर धारणा करता है। यह आज्ञा चक्र का स्थान है। यह भूमध्य में है। यह जाग्रत अवस्था में मन का स्थान है। यदि आप इस स्थान पर धारणा करें, तो आप सरलता से मन को नियन्त्रित कर सकते हैं। यहाँ पर धारणा करने से अत्यन्त शीघ्र ही, यहाँ तक कि एक दिन के अभ्यास से ही कुछ लोगों को प्रकाश दिखायी देने लगता है। वे अभ्यासी जो विराट् पर ध्यान करना चाहते हैं तथा जगत् की सहायता करना चाहते हैं, उन्हें अपने ध्यान हेतु इस स्थान का चुनाव करना चाहिए। एक भक्त को हृदय पर जो कि भावना तथा अनुभव का स्थान है, ध्यान करना चाहिए। जो हृदय पर ध्यान करते हैं, उन्हें महानू आनन्द की प्राप्ति होती है। जो आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें हृदय पर ध्यान करना चाहिए।
एक हठयोगी अपना मन सुषुम्ना नाड़ी जो कि मेरुरज्जु का मध्य मार्ग है तथा किसी विशेष चक्र जैसे मूलाधार, मणिपूर अथवा आज्ञा चक्र पर एकाग्र करता है। कुछ योगी निम्न चक्रों की उपेक्षा करते हैं। वे अपने मन को आज्ञा चक्र पर ही एकाग्र करते हैं। उनका सिद्धान्त यह है कि वे आज्ञा चक्र पर नियन्त्रण के द्वारा सभी निम्न चक्रों पर स्वयं ही नियन्त्रण कर सकेंगे। जब आप किसी चक्र पर धारणा करते हैं, तो प्रारम्भ में मन तथा उस चक्र के मध्य तन्तु जैसा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इसके पश्चात् योगी सुषुम्ना के साथ-साथ एक-एक चक्र ऊपर चढ़ता चला जाता है। यह उत्थान धैर्यपूर्वक प्रयत्न द्वारा शनैः-शनैः होता है । सुषुम्ना के प्रवेश द्वार में हलचल होने से अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होती है। तब आप मदमस्त हो जाते हैं। आप संसार को पूर्णतः विस्मृत कर देंगे। । सुषुम्ना के द्वार में स्पन्दन होने पर कुलकुण्डलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है और अन्तर में महान् वैराग्य आ जाता है। आप पूर्ण निर्भय हो जाते हैं। आपको अनेक दृश्य दिखायी देते हैं। आप श्रेष्ठ अन्तर्ज्योतियों के साक्षी बनते हैं। इसे उन्मनी अवस्था कहते हैं। विभिन्न चक्रों पर नियन्त्रण द्वारा आपको अनेक प्रकार के आनन्द तथा विभिन्न ज्ञान प्राप्त होते हैं— जैसे यदि आपने मूलाधार पर विजय प्राप्त कर ली है, तो आपने भूमण्डल पर स्वयं ही विजय प्राप्त कर ली है। यदि आपने मणिपूर चक्र पर विजय प्राप्त कर ली है, तो आपने अग्नि पर स्वयं ही विजय पा ली है, अब अभि आपको नहीं जला सकती। पंच धारणा आपको पंच तत्त्वों पर विजय में सहायक सिद्ध होगी। इनको किसी दक्ष योगी के निर्देशन में सीखें ।
३. धारणा हेतु निर्देश
मन को किसी एक विचार पर केन्द्रित करना धारणा कहलाती है। धारणा में मन शान्त एवं स्थिर हो जाता है। इसमें मन की विभिन्न किरणें एकत्रित करके ध्यान के विषय पर एकाग्र की जाती हैं। मन लक्ष्य पर केन्द्रित हो जाता है। यहाँ मन का किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा। एक विचार मन को आपूरित कर लेता है। इसमें मन की समस्त ऊर्जाएं एक विचार पर केन्द्रित हो जाती हैं। इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं तथा वे कार्य नहीं करतीं। जब धारणा गहन होती है, तो शरीर तथा वातावरण के प्रति कोई चेतना नहीं रहती। जिसकी अच्छी धारणा होती है, वह पलक झपकते ही, बन्द आँखें किये हुए स्पष्ट रूप से ईश्वर का चित्र देख सकता है।
मनोराज्य (हवाई किले बनाना) को धारणा नहीं कहते। यह मन का हवा में उड़ान भरना है। इसे धारणा अथवा ध्यान समझने की गलती न करें। मन की इस आदत को आत्म-निरीक्षण तथा आत्म-विश्लेषण द्वारा रोकें।
यदि आप अपने मन को किसी बिन्दु पर १२ सेकेंड तक केन्द्रित करते हैं, तो यह धारणा है। ऐसी १२ धारणाएँ मिल कर एक ध्यान होंगी— १२X१२=१४४ सेकेंड | १२ ऐसे ध्यान २५ मिनट २८ सेकेंड एक समाधि होंगे। वह कूर्मपुराण के अनुसार है। भगवान् के चित्र पर भी धारणा को किया जा सकता है।
धारणा तथा प्राणायाम दोनों ही एक-दूसरे पर निर्भर हैं। यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो आपको धारणा प्राप्त होगी। सामान्य रूप से प्राणायाम का अभ्यास धारणा के बाद किया जाता है। अलग-अलग प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न अभ्यास हैं। कुछ लोगों को पहले प्राणायाम का अभ्यास करना सरल पड़ता है, जब कि अन्य को पहले धारणा करना सरल पड़ता है।
जब धारणा गहन हो जाती है, तो आपको बड़े ही आनन्द तथा आध्यात्मिक उन्माद का अनुभव होगा। आप अपने शरीर तथा चारों ओर के वातावरण आदि सबको भूल जायेंगे। सभी प्राण ऊपर सिर की ओर ले जाये जायेंगे ।
प्राणायाम रजोगुण तथा तमोगुण के उस आवरण को हटाता है, जिसने सत्त्व को आवृत कर रखा है। यह नाड़ियों को शुद्ध करता है। यह मन को दृढ़ एवं स्थिर बनाता है, जिससे वह धारणा हेतु तैयार हो जाता है। प्राणायाम से मन की अशुद्धियाँ उसी प्रकार दूर हो जाती हैं, जैसे स्वर्ण को गलाने पर उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं।
जब आप अत्यन्त रुचि के साथ किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो आपको अपना लेकर जोरर-जोर से चिल्ला रहे व्यक्ति की आवाज भी नहीं सुनायी देती। यहाँ तक कि आप अपने सामने खड़े व्यक्ति को भी नहीं देख पाते, अपने पास रखे पुष्पों की सुगन्ध का भी आपको अनुभव नहीं होता। इसे ही धारणा कहते हैं। यहाँ मन एक वस्तु पर दृढ़ता से एकाग्र है। जब आप आत्मा अथवा ईश्वर का चिन्तन करे, तो धारणा ऐसी ही होनी चाहिए। मन को सांसारिक विषय पर केन्द्रित करना बड़ा ही सरल है; क्योंकि मन आदत के कारण स्वाभाविक रूप से इसमें रुचि लेता है। मस्तिष्क में इसकी लीक कटी हुई है। आपको नित्य ही भगवान् अथवा स्वयं के भीतर स्थित आत्मा पर ध्यान के अभ्यास हेतु मन को प्रशिक्षित करना होगा। फिर मन बाह्य विषयों की ओर नहीं जायेगा, क्योंकि इसे धारणा के अभ्यास से अत्यधिक आनन्द प्राप्त होगा।
एक स्वर्णकार एक दस कैरेट स्वर्ण को शुद्ध स्वर्ण में बदलने के लिए इसमें अम्ल मिला कर इसे घरिया में कई बार जलाता है। इसी प्रकार आपको धारणा द्वारा अपने गुरु के निर्देशों तथा उपनिषदों के वाक्यों पर चिन्तन अथवा ध्यान अथवा जप अथवा मानसिक जप द्वारा अपने विषयी मन को शुद्ध करना होगा।
प्रारम्भिक अभ्यासियों को ध्यान में झटकों का अनुभव होता है। सिर पैरो हाथों वक्ष अथवा भुजाओं में झटके लग सकते हैं। भीरु लोग अनावश्यक ही इनसे घबरा जाते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वास्तव में ध्यान मस्तिष्क की कोशिकाओं, नाड़ियों आदि में परिवर्तन लाता है। इसमें पुरानी कोशिकाएँ, नयाँ शक्तिशाली कोशिकाओं द्वारा स्थानान्तरित की जाती हैं। वे सत्त्व से आपूरित हो जाती है। सात्विक विचार तरंगों के लिए नयी लीकों का, नये मार्गों का निर्माण मस्तिष्क तथा मन में होता है, इसी कारण मांसपेशियाँ थोड़ी उत्तेजित हो जाती हैं। साहसी बनें। साधक के लिए साहस एक महत्त्वपूर्ण गुण एवं योग्यता है। इस सद्गुण का अर्जन कीजिए।
सही आसन में बैठें। नेत्रों को बन्द कर लें। कल्पना करें कि सर्वत्र ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है।
जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीजगणित को समझने के लिए अंकगणित का प्रारम्भिक ज्ञान आवश्यक है, संस्कृत के काव्य तथा वेदान्त के ग्रन्थ लघु सिद्धान्त कौमुदी और तर्क संग्रह के प्रारम्भिक ज्ञान के बिना नहीं समझे जा सकते। इसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म पर ध्यान प्रारम्भ में स्थूल प्रतीक के बिना सम्भव नहीं है। दृश्य एवं ज्ञात के द्वारा अदृश्य एवं अज्ञात तक पहुँचने का प्रयास करें।
जितना अधिक आप ईश्वर में मन को एकाग्र करेंगे। आपका मन उतनी ही शक्ति अर्जित करेगा। अधिक धारणा अर्थात् अधिक ऊर्जा। धारणा प्रेम अथवा अनन्तता के साम्राज्य के आन्तरिक प्रकोष्ठों को खोलती है। धारणा ज्ञान के कोष को खोलने की एकमात्र चाबी है।
धारणा करें। ध्यान करें। गहन चिन्तन-शक्ति का विकास करें। अनेक जटिल बिन्दु तब एकदम स्पष्ट हो जायेंगे। आपको अपने भीतर से ही उत्तर एवं हल प्राप्त होंगे।
अपने ज्ञान एवं साक्षात्कार की पुष्टि हेतु शुकदेव जी को राजा जनक के पास जाना पड़ा था। राजा जनक ने अपने दरबार में उनकी परीक्षा ली थी। उन्होंने शुकदेव का ध्यान भटकाने के लिए अपने महल के चारों ओर नृत्य एवं संगीत की सभाएँ आयोजित की और शुकदेव को हाथ में एक दूध से भरा हुआ प्याला ले कर महल के तीन चक्कर लगाने के लिए कहा, लेकिन प्याले से दूध की एक भी बूँद नहीं गिरनी चाहिए थी। शुकदेव जी तो अपनी आत्मा में पूर्ण स्थित थे, इसलिए वे परीक्षा में पूर्ण सफल रहे। कोई भी उनके मन को विचलित नहीं कर सकता था।
धारणा का अभ्यास धीरे-धीरे स्थिरतापूर्वक करें। इसके अभ्यास से आप नरश्रेष्ठ बन जायेंगे।
आपको प्रारम्भ में मन को उसी तरह बहलाना होगा, जिस प्रकार बच्चे को बहलाते हैं। मन भी एक अज्ञानी बच्चे की तरह है। मन से कहें- "अरे मन, तुम मिथ्या निरर्थक नाशवान् वस्तुओं के पीछे क्यों भागते हो? तुम्हें इसमें अनेक कष्ट होंगे। भगवान् कृष्ण की ओर देखो, जो सर्वाधिक सौन्दर्यशाली हैं। इससे तुम्हें नित्य आनन्द की प्राप्ति होगी। तुम संसार के प्रेम गीतों को सुनने के लिए क्यों भागते हो? भगवान् के भजन सुनो। आत्मा को झंकृत करने वाले कीर्तनों को सुनो। तुम्हारा उत्थान होगा।" इस प्रकार मन धीरे-धीरे अपनी पुरानी बुरी आदत को छोड़ देगा और स्वयं भगवान् के चरणों में एकाग्र हो जायेगा। जब यह रजोगुण एवं तमोगुण से मुक्त हो जायेगा, तो यह आपका पथ-प्रदर्शन करेगा। तब यह आपका गुरु होगा।
जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठें, ॐ का तीन से छह बार उच्चारण करें। यह आपके मन से सभी सांसारिक विचारों को दूर करेगा तथा विक्षेपों को दूर हटायेगा। इसके बाद मानसिक रूप से ॐ का जप करें।
सभी अन्य संवेदनात्मक अनुभवों एवं विचारों की उपेक्षा करें। मन के भीतर परस्पर सम्बन्धी कार्यों से उत्पन्न जटिलताओं को रोकें। मन को एक ही विचार पर लगायें ।मन की अन्य सभी गतिविधियों को बन्द कर दें। अब सम्पूर्ण मन एक ही विचार से परिपूर्ण होगा । जिस प्रकार एक ही विचार अथवा एक ही कार्य की पुनरावृत्ति से उस विचार अथवा कार्य में दक्षता आती है, उसी प्रकार एक ही क्रिया अथवा विचार की पुनरावृत्ति से विचारों के एकीकरण, धारणा तथा ध्यान में दक्षता आती है।
प्रारंभ में मन को एक ही विचार पर लगाना अत्यन्त कठिन होगा। विचारों की संख्या में कमी करें। एक ही विषय पर विचार करने का प्रयत्न करें। यदि आप गुलाब के बारे में विचार कर रहे हो, तो मात्र गुलाब से ही सम्बन्धित सभी विचार होने चाहिए। आप संसार के विभिन्न भागों में उगने वाले विभिन्न प्रकार के गुलाबों के बारे में सोच सकते है। निर्मित होने वाली विभिन्न चीजों के बारे में भी विचार कर सकते हैं। मन की निरुद्देश्य रूप से इधर-उधर भटकने की अवस्था को रोकें। गुलाब के बारे में विचार करें, तो निर्थक रूप से आने वाले अन्य विचारों को न रखें । धीरे-धीरे आप मन को मात्र एक ही विचार पर केन्द्रित कर सकेंगे। आपको नित्य ही मन पर संयम करना होगा। विचार-नियन्त्रण हेतु सदैव जागरूक रहना आवश्यक है।" |
कामनाओं तथा आवश्यकताओं में कमी, एक या दो घण्टे नित्य मौन एक एकान्त कमरे में एक या दो घण्टे रहने, प्राणायाम के अभ्यास, प्रार्थना, नित्य ध्यान की बैठकों में वृद्धि तथा विचार आदि के द्वारा धारणा में वृद्धि होती है।
आपको सदैव उत्साहपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण रहने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी आपको मन की धारणा प्राप्त होगी। बराबर वालों के साथ मैत्री, छोटों तथा दुखी करें के प्रति करुणा, गुणी और वरिष्ठ जनों के प्रति मुदिता तथा पापी एवं दुर्जनों के प्रति उपेक्षा के भाव का अभ्यास करने से प्रसन्नता एवं शान्ति उत्पन्न होती है तथा घृणा और ईर्ष्या का नाश होता है।
विचारों की संख्या में कमी से धारणा में वृद्धि होती है। विचारों की संख्या में कमी करना निश्चय ही पहाड़ पर चढ़ने के समान दुष्कर प्रतीत होगा। प्रारम्भ में यह आपको बहुत थका देगा, यह कार्य अरुचिकर भी अनुभव होगा; लेकिन बाद में आपको आनन्द भी देगा, क्योंकि विचारों में कमी से आपको मन की प्रचुर शक्ति तथा आन्तरिक शान्ति प्राप्त होगी। धैर्य, अध्यवसाय, जागरूकता और दृढ संकल्प से सुसज्जित हो कर आप विचारों को सन्तरे अथवा नीबू की भाँति आसानी से कुचल सकेंगे।
इनको कुचलने के बाद इन्हें उखाड़ फेंकना आपके लिए अधिक सरल होगा। इन्हें कुचलना अथवा दबाना मात्र पर्याप्त नहीं होगा। इससे पुनः विचारों का पुनर्जीवन होगा। इन्हें उसी प्रकार पूर्णतया उखाड़ फेंकना चाहिए, जिस प्रकार हिलते हुए दाँत को जड़ से उखाड़ दिया जाता है। मौन धारण, प्राणायाम के अभ्यास, आत्म-संयम, कठोर साधना तथा मानसिक रूप से अधिक निरासक्ति के भाव के अर्जन के द्वारा धारणा का विकास किया जा सकता है।
जाग्रत एवं स्वप्नावस्था के मध्य की सन्धि पर धारणा का अभ्यास एवं इस सन्धि-काल को बढ़ाना दोनों ही कठिन है। रात्रि के समय शान्त कमरे में बैठें और सावधानीपूर्वक मन को देखें। आप सन्धि की स्थिति को प्राप्त करने योग्य हो जायेंगे। तीन माह तक नियमित अभ्यास करें। आपको सफलता मिलेगी।
अपनी गतिविधियों में कमी करें। आपको और अधिक धारणा एवं आन्तरिक जीवन प्राप्त होगा।
यदि आपको कमरे के भीतर मन को एकाग्र करने में कठिनाई का अनुभव हो, तो बाहर आ जायें, खुले स्थान पर, छत पर, नदी के किनारे अथवा बगीचे के शान्त कोने में बैठ जायें। आपकी धारणा अच्छी होगी।
जैसे ही आप टार्च का बटन दबाते हैं, पलक झपकते ही प्रकाश चमकता है। इसी प्रकार योगी धारणा करके आज्ञा चक्र (दोनों भौंहों के मध्य स्थान पर) का बटन दबाता है और तत्काल दैवी प्रकाश चमकता है।
४. अन्तर्मुख एवं बहिर्मुख वृत्तियाँ
अन्तर्मुख- वृत्ति
आपको अन्तर्मुख-वृत्ति मात्र तभी प्राप्त हो सकती है, जब आपने मन को बाहर ले जाने वाली समस्त शक्तियों को नष्ट कर दिया हो। सत्त्व में वृद्धि के कारण मन की ऊर्जा को भीतर की ओर खींचना अन्तर्मुख-वृत्ति है।
आपको योग की क्रिया प्रत्याहार के द्वारा मन को अन्तरावलोकन करने अर्थात् इसको स्वयं की ओर भीतर की ओर मोड़ने की क्रिया को सीखना चाहिए। जिनको इस क्रिया का ज्ञान होता है, वे ही शान्ति से पूर्ण होते हैं तथा मात्र वे ही प्रसन्न रहते हैं। मन में अब किसी प्रकार का विध्वंस नहीं होता। मन अब स्वयं बाहर नहीं निकल सकता ! इसे अब हृदय-गुहा में रखा जा सकता है। त्याग और वैराग्य (कामनाओं, विषयों तथा अहंकार के त्याग) द्वारा आपको मन को भूखा रखना चाहिए।
जब मन की बाहर जाने वाली वृत्तियाँ रोक ली जाती है, जब मन हृदय में ही रुका रहता है, जब इसका पूरा ध्यान स्वयं ही मात्र इसी की ओर ही मुड़ जाता है, तो इस अवस्था को अन्तर्मुख-वृत्ति कहते हैं। जब साधक को यह अन्तर्मुख-वृत्ति प्राप्त हो जाती है, तो वह अधिक साधना कर सकता है। वैराग्य तथा अन्तरावलोकन इस मानसिक अवस्था की प्राप्ति में बड़े ही सहायक होते हैं।
बहिर्मुख वृत्ति
रजोगुण के कारण मन के बाहर की ओर जाने वाली वृत्ति को बहिर्मुख-वृत्ति कहते हैं। पुरानी आदत के प्रभाव से कान और नेत्र तुरन्त बाहर से आती हुई ध्वनि की ओर जाते हैं। विषय और कामनाएँ बाहर की ओर जाने वाली शक्तियाँ है। एक राजसिक मनुष्य अन्तर्मुख-वृत्ति वाले अन्तर आध्यात्मिक जीवन का स्वप्न भी नहीं देख सकता । वह अन्तरावलोकन हेतु पूर्ण अयोग्य है।
जब दृष्टि बाहर की ओर जाती है, तो बदलते हुए परिदृश्य मन को आपूरित कर लेते हैं। मन की बाहर जाने वाली ऊर्जाएं कार्य करने लगती हैं।
जब आप इस विचार पर पूर्ण स्थापित हो जाते हैं कि जगत् असत्य है, तो विक्षेष (जो कि नाम और रूपों के कारण है) तथा संकल्पों का स्फुरण धीरे-धीरे नष्ट होता है। इस सूत्र को निरन्तर दोहरायें : “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या – ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जगत् मिथ्या है। जीव ब्रह्म के साथ एक है।” इससे आपको प्रचुर शक्ति और मन की शान्ति प्राप्त होगी।
५. मन के मार्गों को जानें
धारणा का अभ्यास मन के रूपान्तरणों को रोकने के लिए किया जाता है।
मन को एक रूप अथवा विषय पर लम्बे समय तक स्थिर रखना एकाग्रता है।
क्षिप्त, मूढ, विक्षेप, एकाग्र तथा निरुद्ध—ये पाँच यौगिक भूमिकाएँ हैं। चित्त अथवा मन पाँच विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। क्षिप्त अवस्था में मन की किरणें विभिन्न विषयों पर फैली हुई रहती हैं। यह बेचैन रहता है तथा एक विषय से दूसरे विषय पर कूदता रहता है। मूढ अवस्था में मन सुस्त और भुलक्कड़ होता है। विक्षिप्त अवस्था मन का एकत्रीकरण है, यह यदा-कदा स्थिर रहता है और कभी-कभी यह विभ्रान्त रहता है। धारणा के अभ्यास से मन स्वयं ही एकाग्र होने के लिए यत्नशील होता है। एकाग्र अवस्था में यह केन्द्रित होता है। तब मन में मात्र एक ही विचार उपस्थित होता है। निरुद्ध अवस्था में मन नियन्त्रण में होता है।
मन के भीतर बहिर्गामी एवं विषयाश्रित शक्तियाँ हैं। ये इसे बहिर्मुख वृत्ति की ओर ले जाती है। मन विषयों की ओर खींचता है। निरन्तर साधना (आध्यात्मिक साधना से मन को बहिर्गामी होने से रोका जाता है। इसे ब्रह्म की ओर इसके वास्तविक गृह की ओर मोड़ा जाना चाहिए।
मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक यह केन्द्रित होगा, उतनी ही अधिक देर तक यह एक बिन्दु पर एकाग्र होने की शक्ति एकत्र करेगा। विभिन्न विषयों पर बिखरी मन की किरणों को एकत्रित करके मन को ईश्वर पर केन्द्रित करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। यह आपका महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। आप अपना कर्तव्य भूल गये है। आप परिवार, बच्चों, धन, शक्ति, पद, नाम तथा प्रसिद्धि के प्रति मोह के कारण अपना कर्तव्य भुला बैठे हैं।
मन की तुलना पारे के साथ की जाती है, क्योंकि इसकी किरणें विभिन्न विषयों पर बिखरी रहती हैं। इसकी तुलना बन्दर के साथ की जाती है, क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय पर कूदता रहता है। इसकी तुलना भ्रमण करती हुई वायु से की जाती है, क्योंकि यह चंचल है। मन की कामुक प्रचण्डता के कारण इसकी तुलना कामुक क्रोधोन्मत्त हाथी से की जाती है।
मन को बड़ी चिड़िया भी कहते हैं; क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय पर उसी तरह कूदता रहता है, जिस तरह चिड़िया एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकती रहती है। मन को कैसे एकाग्र किया जाये और फिर मन की अन्तरतम गुहाओं की खोज कैसे की जाये, राजयोग इसकी शिक्षा देता है।
धारणा विषय-वासनाओं की विरोधी हैं, आवेश और चिन्ताओं के लिए. आनन्द है। यह व्याकुलता में स्थिर चिन्तन देती है। आलस्य एवं जड़ता के स्थान पर व्यावहारिक चिन्तन प्रदान करती है। बुरी भावनाओं के स्थान पर परमानन्द प्रदान करती है।
जब तक स्थिर अभ्यास के द्वारा विचार पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते, तब तक उसे अपने मन को एक समय में एक ही सत्य पर केन्द्रित करना होगा। इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करने से मन को एक बिन्दु पर एकाग्र होने की क्षमता प्राप्त होगी और तत्क्षण विचारों की सेना समाप्त हो जायेगी।
मन के इस विचलन तथा विभिन्न अन्य विघ्नों, जो कि मन की एकाग्रता के मार्ग में खड़े हैं, को दूर करने के लिए धारणा का अभ्यास ही एकमात्र उपाय है।
मन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी सुखकर अथवा रुचिकर विषय से संयुक्त रहता है। एक उदाहरण देखिए जब आप गुलमर्ग, सोनमर्ग, चश्मेशाही और अनन्तनाग के सुन्दर दृश्यों का आनन्द ले रहे होते हैं, उसी समय यदि आपको अपने एकमात्र पुत्र के असामयिक निधन का समाचार मिलता है, तो आपका मन एकदम से व्यथित हो जाता है। अब आपको सुन्दर दृश्यावलि में कोई रुचि नहीं रह जाती। यहाँ अवधान का उच्चाटन हो गया है। अब आपके मन में निराशा है। ये धारणा और एकाग्रता ही है, जो आपको दृश्य देखने में आनन्द प्रदान करती हैं।
ध्यान बिन्दु उपनिषद् में लिखा है-"आत्मा को मथनी का निचला भाग तथा प्रणव को मथनी का ऊपरी भाग बना कर व्यक्ति को मन्थन (जिसे ध्यान कहते हैं) के अभ्यास द्वारा एकान्त में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए।"
अपने सामने भगवान् ईसामसीह का चित्र रखें। ध्यान के अपने प्रिय आसन में बैठ जायें। चित्र के ऊपर सहज रूप से तब तक धारणा करें, जब तक आपके नेत्रों से अश्रु न बहने लगे। अपने मन को उनके वक्षस्थल के ऊपर क्रास, लम्बे बालों, सुन्दर दाढ़ी, गोल नेत्रों तथा अन्य अंगों और उनके सिर के चारों ओर निकल रहे आध्यात्मिक आभामण्डल के ऊपर घुमायें। उनके दैवी गुणों जैसे प्रेम, उदारता, करुणा और धैर्य के बारे में विचार करें।
मन को बाह्य वस्तुओं पर एकाग्र करना सरल होता है। मन की बाहर की ओर जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कामना भावोत्तेजक मन का एक प्रकार है। इसके पास मन को बहिर्मुखी करने की शक्ति है।
मन को आत्मा पर लगायें। इसे सर्वव्यापक शुद्ध बुद्धि और स्वज्योति पर केन्द्रित करें। ब्रह्म में दृढ़ रहें। तब आप ब्रह्मस्थ (ब्रह्म में स्थित) हो जायेंगे।
मन की धारणा का अभ्यास करें। मन को एक विचार, एक विषय पर केन्द्रित करे मन जब अपने लक्ष्य से दूर भागे, तो इसे बार-बार वापस खींचें और लक्ष्य पर पुनः केन्द्रित करें। मन को विचारों के सैकड़ों रूप न निर्मित करने दें। आत्म-निरीक्षण करें और मन को सावधानीपूर्वक देखें। अकेले रहें। संगति से बचें। अधिक लोगों के साथ घुलें मिलें नहीं। यह महत्त्वपूर्ण है। मन को व्यर्थ के विचारों, व्यर्थ चिन्ताओं, व्यर्थ कल्पनाओं, व्यर्थ भय तथा व्यर्थ पूर्वानुमानों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न गँवाने दें। निरन्तर अभ्यास द्वारा अपने मन को किसी विचार के एक रूप पर आधे घण्टे तक केन्द्रित करें। मन को स्वयं ही एक आकार का होने देने का प्रयास करें और निरन्तर अभ्यास के द्वारा इसे उसी आकार का बनाये रखने का प्रयास करें।
अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते समय आप देखेंगे कि इस समय आपको स्वयं ही अपने मन में प्रतिबिम्ब बनाने की आवश्यकता का अनुभव होगा, लेकिन आप इसकी सहायता नहीं कर सकते।
ध्यान के समय मन के साथ संघर्ष न करें। यह एक भयंकर भूल है। कई नवाभ्यासी यह भयंकर गलती करते हैं। यही कारण है कि वे शीघ्र थक जाते हैं। उनका सिर दर्द करने लगता है अथवा ध्यान के समय मेरुरज्जु में मूत्रण केन्द्र में उत्तेजना होने के कारण, उन्हें अति शीघ्र मूत्र त्याग हेतु उठना पड़ता है। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन अथवा स्वस्तिक आसन में आराम से बैठ जायें। सिर, गर्दन और वक्ष को एक सीधी रेखा में रखें। मांसपेशियों, नाड़ियों तथा मस्तिष्क को शिथिल करें। विषयी मन को शान्त करें। नेत्र बन्द करें। प्रातः काल ४ बजे (ब्राह्ममुहूर्त में) जागें। मन के साथ संघर्ष न करें। इसे शान्त और शिथिल रखें।
मन को कुशलतापूर्वक प्रशिक्षित करने से आप इस पर नियन्त्रण प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसा चाहें, इससे वैसा कार्य करवा सकते हैं तथा यदि आप चाहें, तो इसे उसकी शक्तियाँ प्रयोग करने के लिए विवश कर सकते हैं।
उच्च योगियों में आप कह नहीं सकते कि कहाँ प्रत्याहार समाप्त होता है और धारणा प्रारम्भ होती है, कहाँ धारणा समाप्त होती है और ध्यान प्रारम्भ होता है तथा कहाँ ध्यान समाप्त होता है और समाधि प्रारम्भ होती है। जिस क्षण वे आसन में बैठते हैं, सभी क्रियाएँ विद्युत् गति से स्वयं ही सम्पादित होने लगती हैं और वे अपनी इच्छा से समाधि में प्रविष्ट हो जाते हैं। नवाभ्यासियों में सर्वप्रथम प्रत्याहार स्थान लेता है। इसके बाद धारणा प्रारम्भ होती है। तत्पश्चात् धीरे से ध्यान आता है। समाधि प्रारम्भ होने के पहले उनके मन अधैर्यवान हो जाते हैं तथा वे थक जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। निरन्तर प्रबल साधना हल्के किन्तु पौष्टिक आहार के साथ करने से साधना में आशाजनक सफलता प्राप्त होती है।
जिस प्रकार एक कुशल तीरन्दाज एक चिड़िया का शिकार करने के लिए इस बात का ध्यान रखता है कि वह किस ओर आगे बढ़ेगा, कैसे अपना धनुष उठायेगा किस प्रकार कमान खींचेगा और किस समय चिड़िया के ऊपर तीर छोड़ेगा अर्थात इस स्थिति में खड़े रह कर, इस प्रकार धनुष पकड़ कर, इस प्रकार कमान खींच कर, बाण को छोड़ कर, मैं चिड़िया को बींधूंगा।' और इसके बाद वह कभी भी इन स्थितियों को बनाने में और लक्ष्य को वेधने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार साधक को भी इन स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए जैसे 'इस प्रकार का भोजन ले कर, इस गुरु का अनुकरण करके, इस समय मैं ध्यान और समाधि प्राप्त करूँगा।'
एक चतुर रसोई बनाने वाला अपने मालिक की सेवा करने के लिए, उस भोजन का ध्यान रखता है, जो उसके मालिक को रुचिकर लगता है और इस प्रकार सेवा करने से उसे लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार साधक को भी ध्यान और समाधि की प्राप्ति तथा उनके आनन्द को बार-बार प्राप्त करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पोषण आदि।
हठयोगी अपनी श्वास को प्राणायाम द्वारा नियन्त्रित करके अपने मन को एक करने का प्रयास करता है, जब कि राजयोगी चित्तवृत्तिनिरोध (अर्थात् मन को विषयों को विभिन्न आकारों को ग्रहण करने से रोकना) के द्वारा अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करता है। वह श्वास के नियन्त्रण की चिन्ता भी नहीं करता; लेकिन जब उसका मन नियन्त्रित हो जाता है, तो उसकी श्वास स्वयं ही नियन्त्रित हो जाती है। हठयोग राजयोग की ही एक शाखा है।
सांसारिक सुख सुख का उपभोग करने की इच्छा को तीव्र करते हैं। इसी कारण सांसारिक व्यक्तियों के मन अत्यधिक बेचैन होते हैं। उनके मन में किंचित् भी सन्तोष तथा मानसिक शान्ति नहीं होती। चाहे आप कितने भी सुख इसके लिए संग्रहित करके रखें, मन कभी सन्तुष्ट नहीं होगा। जितना अधिक आप सुखों का उपभोग करेंगे, उतना ही अधिक यह उनकी माँग करता है। इसीलिए लोग अपने मनों के कारण ही अत्यधिक परेशान रहते हैं। वे अपने मनों से थक चुके हैं, अतः इन परेशानियों को दूर करने के लिए ऋषियों ने विचार किया कि मन को सभी विषय-सुखों से वंचित रखा जाना चाहिए जब मन एकाग्र अथवा नष्ट कर दिया जायेगा, तो यह व्यक्ति को आगे सुखों की खोज हेतु कचोटेगा नहीं और सभी कष्ट एवं परेशानियाँ सदा के लिए ही दूर हो जायेंगी और उसे सच्ची शान्ति प्राप्त होगी।
सांसारिक व्यक्तियों में मन की किरणें छितरी रहती हैं। उनमें मन की ऊर्जा का विभिन्न दिशाओं में अपव्यय होता है। धारणा के लिए इन बिखरी हुई किरणों को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा एकत्र करना चाहिए और फिर मन को ईश्वर की ओर मोड़ा जाना चाहिए।
मन की शक्तियाँ प्रकाश की किरणों की तरह होती है। ये विभिन्न विषयों की ओर खिंचती हैं। आपको इनको वैराग्य और अभ्यास के द्वारा, त्याग और तपस्या के द्वारा एकत्र करना चाहिए और फिर इस अक्षय ऊर्जा के साथ ईश्वर अथवा ब्रह्म की ओर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब मानसिक किरणें एकाग्र की जाती हैं, तो ज्ञान आता है।
रजोगुण और तमोगुण जो सत्त्व को आवृत किये हैं, उनका उन्मूलन प्राणायाम, जप, , विचार और भक्ति के द्वारा करें। तब मन धारणा हेतु तैयार हो जायेगा।
जब आप सदैव उत्साहित रहें, जब आपका मन सन्तुलित और एकाग्र हो, तो जानें कि आप योग में प्रगति कर रहे हैं।
६. मन की घुमन्तु प्रवृत्ति को कम करें
एक वैज्ञानिक अपने मन को एकाग्र करता है और अनेक वस्तुओं का आविष्कार करता है। धारणा के द्वारा वह स्थूल मन की पर्तों को अनावृत करता है और मन के उच्च क्षेत्रों में गहरे तक प्रविष्ट हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करता है। वह मन की सभी शक्तियों को एकत्रित करके उन्हें उन पदार्थों पर डालता है, जिनका वह विश्लेषण कर रहा है। इस प्रकार वह उनके रहस्यों को खोज निकालता है।
जिसने मन का कुशलतापूर्वक उपयोग करना सीख लिया है, सम्पूर्ण प्रकृति उसके नियन्त्रण में होती है।
जब आप अपने किसी प्रिय मित्र को छह वर्ष पश्चात् देखते हैं, तो जो आनन्द आपको प्राप्त होता है, वह आपको उस व्यक्ति से नहीं प्राप्त होता, वरन् स्वयं अपने भीतर से प्राप्त होता है। मन उस समय एकाग्र हो जाता है और आप स्वयं अपने भीतर स्थित आत्मा से आनन्द प्राप्त करते हैं।
जब मन की किरणें विपरीत विषयों पर बिखरी हुई रहती हैं, तो आपको दुःख प्राप्त होता है। जब अभ्यास के द्वारा ये किरणें एकत्रित हो जाती हैं, तो मन एकाग्र हो जाता है और आपको अपने भीतर से आनन्द प्राप्त होता है।
जब मन का विकास होता है, तो आप पास अथवा दूर स्थित, जीवित अथवा मृत अन्य लोगों के साथ सजगतापूर्वक सम्पर्क में आते हैं।
जब मन में विश्वास होता है, तो जिस विषय को आप समझना चाहते है उस पर सरलता से एकाग्र हो जाता है और वह जल्दी से समझ में आ जाता है।
यदि आपको अपने मन को हृदय, त्रिकुटी अथवा सिर के शीर्ष पर एकाग्र करने में कठिनाई का अनुभव हो, तो आप किसी बाह्य विषय पर धारणा कर सकते हैं। आप नीले आसमान, सूर्य के प्रकाश, सर्वव्यापक वायु अथवा आकाश, सूर्य, चन्द्र अथवा तारों पर भी धारणा कर सकते हैं।
यदि आपको सिर में दर्द होने लगे, तो आप शरीर के बाहर किसी विषय पर धारणा करने लगें।
यदि आपको आँखों को ऊपर करके त्रिकुटी पर धारणा करने से सिर में दर्द होने लगे, तो तुरन्त अभ्यास बन्द कर दें। हृदय पर धारणा करें।
मन शब्दों तथा उनके अर्थ के बारे में विचार करता है, जब कि अन्य समय में यह विषयों के बारे में विचार करता है। जब आप मन की एकाग्रता चाहते हैं, तो आपको यह प्रयत्न करना होगा कि मन विषयों तथा शब्दों और उनके अर्थ के बारे में विचार नहीं करे।
मेडिकल के कुछ विद्यार्थी प्रवेश लेने के कुछ समय बाद ही घावों की पीब साफ करने तथा मृत शरीर के प्रति घृणा के कारण पढ़ायी बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं। यह एक भयंकर भूल है। प्रारम्भ में यह घृणित अनुभव होता है; किन्तु रोग विज्ञान, औषधियों, शल्य क्रिया, रुग्ण अंगों की संरचना तथा जीवाणु विज्ञान के अध्ययन के बाद अन्तिम वर्ष के पाठ्यक्रम में रुचिकर लगने लगता है। अनेक आध्यात्मिक साधक मन की धारणा का अभ्यास कुछ समय के पश्चात् छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें वह अभ्यास कठिन प्रतीत होता है। वे भी चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों की तरह ही गलती करते हैं। अभ्यास के प्रारम्भ में जब आप शारीरिक चेतना से मुक्त होने हेतु संघर्ष करते रहते हैं, तो यह अरुचिकर तथा कष्टप्रद प्रतीत होगा। यह एक शारीरिक दंगल होगा। मन में अनेक आवेग और संकल्प होंगे। अभ्यास के तृतीय वर्ष में मन शान्त, शुद्ध और दृढ़ बन जायेगा। आपको अत्यधिक आनन्द प्राप्त होगा। ध्यान से प्राप्त आनन्द से तुलना की जाये, तो संसार के समस्त सुख कुछ भी नहीं हैं। किसी भी मूल्य पर अभ्यास न छोड़ें। आगे बढ़ें। अध्यवसाय करें। धैर्य, उत्साह और साहस रखें। अन्ततः आप आगे बढ़ेंगे। कभी निराश न हो। गहन आत्म-निरीक्षण द्वारा उन रुकावटों को ढूंढ निकालें, जो आपके ध्यान में रोड़े की भाँति कार्य करती है और धैर्यपूर्वक प्रयत्न करके उन्हें एक-एक करके दूर करें। नये संकल्पों तथा वासनाओं को जन्म न लेने दें। विवेक, विचार और ध्यान द्वारा उन्हें कलिकावस्था में ही नष्ट कर दें।
इन्द्रियों पर नियन्त्रण तथा मन की धारणा में मनुष्य का कर्तव्य निहित है।
एक तीर बनाने वाला व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त था। वह अपने कार्य में इतना तल्लीन था कि उसे उसकी दूकान के सामने से निकल रही राजा की सवारी का भी पता ही न चला। जब आप अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगायें, तो आपकी एकाग्रता भी ऐसी ही होनी चाहिए। आपके मन में एकमात्र ईश्वर का ही विचार होना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मन की सम्पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। आपको मन की एकाग्रता प्राप्त करने हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। श्री दत्तात्रेय महाराज ने इस तीर बनाने वाले को अपना गुरु माना था।
यहाँ तक कि यदि ध्यान के अभ्यास के समय भी मन बाहर भागे, तो भी चिन्ता न करें। इसे भागते रहने दें। धीरे से इसे अपने लक्ष्य (केन्द्र) की ओर लाने का प्रयत्न करें। बार-बार अभ्यास करने से अन्त में यह आपके हृदय में, आपके हृदय की अन्तर्वासी आत्मा जो कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य है, पर केन्द्रित हो जायेगा। प्रारम्भ में मन शायद ८० बार भागेगा। ६ माह पश्चात् शायद यह ७० बार भागेगा। एक वर्ष पश्चात् यह ५० बार भागेगा। २ वर्ष पश्चात् शायद यह ३० बार भागेगा। ५ वर्षों के बाद यह पूर्णतः दैवी चेतना में स्थित हो जायेगा। इसके पश्चात् यदि आप अपना पूरा प्रयास इसे बाहर लाने के लिए करें, तो भी यह बाहर नहीं भागेगा, उस बिगड़े हुए बैल की तरह, जिसको दूसरों के खेत चरने की आदत थी और अब अपने ही खेत में ताजे चने और बिनौले खाने लगता है।
मन की किरणों को एकत्रित कीजिए। जब आपका कपड़ा किसी झाड़ी में उलझ जाता है, तो आप जिस प्रकार उसमें से धीरे-धीरे एक-एक करके काँटे निकालते हैं. उसी प्रकार आपको अनेक वर्षों से विषय वस्तुओं पर फैली हुई मन की किरणों को सावधानी और प्रयत्नपूर्वक पुनः एकत्रित करना होगा।
आपकी पीठ पर दर्द तथा सूजन होने पर भी रात्रि में जब आप सोये रहते हैं, तो आपको किसी प्रकार के दर्द का अनुभव नहीं होता। मात्र तभी आपको दर्द का अनुभव होता है, जब मन नाड़ियों तथा विचार द्वारा रोगी अंग से संयुक्त रहता है। यदि आप मन को रोगी अंग से सजगतापूर्वक हटा कर ईश्वर अथवा किसी अन्य आकर्षक विषय पर केन्द्रित करें, तो आपको पूर्णतः जाग्रत अवस्था में भी किसी प्रकार के दर्द का अनुभव नहीं होगा। यदि आपमें दृढ़ इच्छा शक्ति तथा तितिक्षा (सहन-शक्ति) होती है, तो भी आपको किसी प्रकार के दर्द का अनुभव नहीं होता। किसी प्रकार के दर्द अथवा कष्ट का निरन्तर चिन्तन करते रहने के द्वारा आप अपने दर्द अथवा रोग में वृद्धि ही करते हैं।
७. सभी शक्तियों का दोहन करें
१. मनुष्य के द्वारा किसी भी चाहे गये लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले सभी संघर्षों तथा प्रयत्नों में, वास्तव में उसे सहायता हेतु किसी बाहरी शक्ति को खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य के स्वयं के भीतर बृहत् संसाधन एवं अन्तर्निष्ठ शक्तियाँ निहित हैं, जिनका कि अभी तक दोहन नहीं किया गया है अथवा वे अभी तक मात्र आंशिक रूप से प्रयोग में लायी गयी हैं।
२. ऐसा इसलिए है, क्योंकि उसने अपनी क्षमताओं को सैकड़ों विभिन्न वस्तुओं पर बिखरा रखा है और इसी कारण इतनी महान् अन्तर्निष्ठ शक्तियों के होते हुए भी वह किसी महान् लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है। यदि वह बुद्धिमत्तापूर्वक उनका नियमन करे और उनका प्रयोग करे, तो शीघ्र और ठोस परिणाम प्राप्त होंगे।
३. शक्तियों के बुद्धिमत्तापूर्वक तथा सफलतापूर्वक उपयोग के लिए मनुष्य को स्वयं के निर्देशन के लिए किसी प्रकार की नयी विधियों की खोज हेतु प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के आरम्भ के समय से ही मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायता हेतु प्रकृति में स्वयं ही प्रचुर मात्रा में प्रेरणाप्रद उदाहरण और शिक्षाएँ है। अवलोकन हमें बताता है कि प्रकृति में प्रत्येक बल को जब स्वच्छन्द रूप से विस्तृत क्षेत्र में प्रवाहित होने दिया जाता है, तो यह सीमित निकास तुलना में कम शक्ति से प्रवाहित होता है।
४. फैली हुई किरणों का एकत्रीकरण तथा इस बल को एक दिये हुए बिन्दु – किसी विषय, विचार अथवा क्रिया पर लाना ही धारणा है।
५. शक्ति की धारणा के द्वारा उत्पन्न बल के बारे में नीचे उदाहरण दिये जा रहे हैं.
● (१) जब नदी विस्तृत स्थान पर बहती है, तो इसका बहाव धीमा रहता है; लेकिन जब इसे एक नहर में से बहाया जाता है, तो यह आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति से बहती है।
● (२) एक भारी बोगी जिसमें टनों वजन रहता है, वह इंजन के बायलर में एकत्रित भाप की शक्ति के द्वारा ले जायी जाती है।
● (३) एक अत्यन्त सामान्य उदाहरण---जब पानी उबलने लगता है, तो भाप से तपेली का ढक्कन हिलने लगता है और गिर जाता है।
● (४) सूर्य की किरणें जो सामान्य गर्म रहती हैं, वे किसी लेंस द्वारा केन्द्रीभूत करने पर अचानक इतनी अधिक गर्म हो जाती है कि वे वस्तुओं को जला देती है। एक सरल और सामान्य क्रिया-जब कोई इस नियम का अनजाने ही प्रयोग करता है—देखने में आती है, जब कोई अपने से कुछ दूर स्थित व्यक्ति को आवाज देना चाहता है, तो वह अपने दोनों हाथों को मुँह के पास ला कर आवाज देता है।
६. यह नियम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से प्रयोग में आता है। शल्य चिकित्सक को ऑपरेशन करने के लिए अत्यधिक एकाग्रता और सावधानी की आवश्यकता होती है। गहन तल्लीनता किसी टेक्नीशियन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट तथा एक कुशल चित्रकार को चित्र बनाने में अथवा योजना बनाने में त्रुटि रहित होना सर्वाधिक आवश्यक है, अतः यहाँ भी एकाग्रता होना प्रथम आवश्यकता है। एक स्विस घड़ी निर्माता को भी घड़ी तथा विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण के छोटे-छोटे पुर्जे बनाने के लिए इसी प्रकार की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ऐसा ही प्रत्येक कला और विद्या में है।
७. आध्यात्मिक क्षेत्र में, जहाँ उसे आन्तरिक शक्तियों के साथ व्यवहार करना होता है, साधक को विशेष रूप से धारणा की आवश्यकता होती है। मन की शक्तियाँ जो कि सदैव बिखरी रहती हैं, वे धारणा में बाधक बनती हैं। यह दोलनात्मक प्रवृत्ति मन तत्त्व का स्वाभाविक लक्षण है। मन के भटकाव को रोकने अथवा कम करने की विभिन्न विधियों में से दृष्टि और श्रव्य का माध्यम प्रमुख है; क्योंकि ये दोनों ही मन को स्थिर करने तथा ध्यान खींचने में कुशल हैं। ऐसा हम एक सम्मोहन करने वाले के विषय में देखते हैं। वह जिसे सम्मोहित करता है, उसे स्वयं (सम्मोहनकर्ता) की आँखों में एकटक देखने के लिए तथा उसके निर्देशों का पालन करने के लिए कहता है। अन्य उदाहरण, जब माँ अपने बच्चे को गोद में ले कर लोरी सुनाती है। एक स्कूल का शिक्षक जब कोई महत्त्वपूर्ण बात पर बच्चों का ध्यान खींचना चाहता है, तो वह कहता है- " अब सारे बच्चे इधर देखेंगे।" वह सोचता है कि इससे वह उनकी दृष्टि को स्वयं पर केन्द्रित करके उनका ध्यान पढ़ायी में एकाग्र कर सकेगा।
इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में धारणा के विकास की विधियों में यह बिन्दु पर या ॐ पर या किसी मन्त्र अथवा किसी देवता के चित्र पर त्राटक (किसी वस्तु को अपलक देखना) का रूप ले लेती है। अन्य लोगों में यह कार्य किसी मन्त्र के जप अथवा किसी प्रकार के कीर्तन द्वारा किया जाता है। इन साधनों के द्वारा मन शनैः-शनै: अन्तर्मुखी और केन्द्रित होता है। जैसे-जैसे यह स्थिति गहन होती जाती है, व्यक्ति शनैः-शनै अपने आस-पास के वातावरण के प्रति अचेतन होता जाता है। यह धारणा अब निरन्तर चलती रहती है, तो यह ध्यान की स्थिति को प्रेरित करती है, जहाँ व्यक्ति अपने शरीर को भी भूल जाता है।
ध्यान जब दृढ़ और पूर्णकालीन हो जाता है, तो इसके द्वारा समाधि (जो कि आत्म चेतना की अन्तिम स्थिति है) अथवा आत्म-साक्षात्कार का अनुभव होता है।
८. धारणा की कहानी
धारणा का अभ्यास प्रारम्भ करने के पूर्व आपको अचेतन मस्तिष्क और इसके कार्यों के बारे में जानना आवश्यक है।
जब चित्त वर्ष में होता है और किसी विशेष बिन्दु पर केन्द्रित होता है, तो वह धारा कहलाती है। आपके अवचेतन मन का अधिकांश भाग दमित अनुभवों का पुंज का है। इसे धारणा के साधन द्वारा चेतन मन की सतह पर लाया जाता है।
यह मनोवैज्ञानिक तथ्य स्वीकार कर लिया जा चुका है कि वह मनोवैज्ञानिक क्रिया-विधि जिसके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, चेतना के धरातल पर समाप्त नहीं होती है; बल्कि वह अवचेतन मन तक भी जाती है। यदि आपको अवचेतन मन से वार्तालाप करने की विधि ज्ञात हो तथा यदि आपको अपने दास अथवा किसी पुराने प्रिय मित्र की भाँति इससे कार्य करवाने की कला और विद्या का ज्ञान हो, तो सम्पूर्ण ज्ञान आपका होगा। बस, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है और अभ्यास आपको इस कला में निपुण बनाता है।
जब कभी आप अध्यात्मविद्या, विज्ञान अथवा दर्शन शास्त्र की किसी पहेली को सुलझाने में असमर्थ रहते हैं, तो आप पूर्ण विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन को अपने लिए थोड़ा कार्य करने के लिए कहें, आपको सही हल निश्चित ही प्राप्त होगा अपने अवचेतन मन को इस प्रकार आदेश दें- "मुझे इस पहेली अथवा समस्या का हल कल सुबह अति शीघ्र चाहिए है, कृपया इसे अति शीघ्र कर दो।" आपका आदेश एकदम स्पष्ट होना चाहिए तथा इसके बारे में आपको किंचित् भी सन्देह नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्रश्न का उत्तर अगली सुबह निश्चित ही प्राप्त हो जायेगा। लेकिन कभी-कभी आपका मन व्यस्त रहता है, इसलिए आपको कुछ दिनों की प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। तब आपको निश्चित समय पर अपना आदेश नियमित रूप से दोहराना पड़ेगा।
वह सब जो आपने स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया है, जो आप पिछले असंख्य जन्मों में ले कर आये हैं, वह सब जो आपने इस जीवन अथवा पिछले जीवन में देखा-सुना, जिस आनन्द का अनुभव किया, जिसे चखा, पढ़ा अथवा जाना है, वह आपके अवचेतन मन में छिपा हुआ है। आप धारणा में तथा अपने अवचेतन मन को आदेश देने में निपुणता क्यों नहीं प्राप्त करते और इस सम्पूर्ण ज्ञान का मुक्तहस्त से उपयोग क्यों नहीं करते?
जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है कि आपका अवचेतन मन आपका विश्वसनीय दास है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब आप रात्रि में सोते समय विचार करते हैं कि मुझे रेल पकड़ने अथवा ध्यानाभ्यास के लिए कल सुबह ४ बजे जागना है, तो यह आपका अवचेतन मन है जो आपको सही समय पर जगा देता है। चाहे आप गहरी नींद में सोये हों, आपका अवचेतन मन सदा कार्य करता रहता है। यह क्षण-भर को भी नहीं सोता। यह उस समय तथ्यों की छानबीन करता है, उनको जमाता है, उनका विश्लेषण करता है और तुलना करता है तथा आपके आदेश का पालन करता है।
प्रत्येक कार्य, सुख अथवा दुःख और वास्तव में सभी अनुभव आपके अवचेतन मन के कैमरे की प्लेट पर रह जाते हैं, यही सूक्ष्म संस्कार हैं जो आपके पुनर्जन्म, सुख और दुःखों के अनुभव और पुनः मृत्यु के कारण है। इस जन्म में किसी कर्म की पुनरावृत्ति आपकी स्मृति को प्रेरित करती है। लेकिन उच्च योगी में पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहती है। वह अपने भीतर गहरे डूब जाता है और पिछले जन्म के संस्कारों के वास्तविक सम्पर्क में आता है। अपने योग-चक्षु से वह उन्हें प्रत्यक्ष देखता है। योग संयम (धारणा, ध्यान तथा समाधि का एक साथ एक ही समय पर अभ्यास) का अभ्यास करने से योगी को पूर्व जन्मों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अन्यों के संस्कारों पर संयम करने से अन्यों के पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। धारणा की शक्तियाँ अद्भुत हैं।
मन आत्मा की शक्ति से जन्मा है, क्योंकि ईश्वर मन के द्वारा ही स्वयं को नाम और रूपों के विश्व के रूप में प्रकट करते हैं। मन और कुछ नहीं, विचारों और आदतों का पुंज है। जिस प्रकार 'मैं' का विचार सभी विचारों का मूल है, मन वह विचार 'मैं' है।
जाग्रत अवस्था में मन का स्थान मस्तिष्क है। स्वप्नावस्था में इसका स्थान प्रमस्तिष्क है तथा सुषुप्ति में इसका स्थान हृदय है। सभी विषय जो आप देखते हैं, वे रूपों अथवा पदार्थ के रूप में मन ही है। मन ही सृष्टि करता है, मन ही नाश करता है। उच्च विकसित मन निम्न मनों को प्रभावित करता है। दूरस्थ व्यक्ति के मन की बात जान लेना, मन को पढ़ना, सम्मोहन, दूरस्थ उपचार तथा अन्य इसी प्रकार की विद्याएँ इस तथ्य का प्रमाण है। निस्सन्देह मन इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी शक्ति है। मन का नियन्त्रण सभी शक्तियाँ प्रदान करता है।
जिस प्रकार व्यायाम करते हैं. टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, उसी प्रकार सात्विक भोजन ग्रहण करना, निर्दोष प्रकृति का सृजन, विचारों में परिवर्तन, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और पवित्र विचारों द्वारा मन का शिथिलीकरण तथा प्रसन्न रहने की आदत का विकास करने के द्वारा आपको मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए।
मन की प्रकृति ऐसी है कि वह जिस पर भी प्रबलता से विचार करता है, वैसा हो बन जाता है। इसलिए आप किसी अन्य व्यक्ति के दुर्गुणों अथवा दोषों के बारे में विचार करते हैं, तो उस समय के लिए आपका मन उन दुर्गुणी अथवा दोषों से आवेशित हो जाता है। जो इस मनोवैज्ञानिक नियम को जानता है, वह कभी भी अन्यों की निन्दा नहीं करता और न ही वह अन्यों के चरित्र में दोष निकालता है। वह सदा दूसरों की प्रशंसा करता है। वह उनमें मात्र अच्छाई का ही दर्शन करता है। धारणा, योग तथा आध्यात्मिकता में प्रगति का यही उपाय है।
मन भारतीय तर्क शास्त्र के अनुसार आणविक है, राजयोग दर्शन के अनुसार यह सर्वव्यापक है, वेदान्त के अनुसार यह शरीर के समान आकार का है।
गहन निद्रा अकर्मण्यता की स्थिति नहीं है। इस अवस्था में कारण शरीर तेजी से कार्य करता है। संयुक्त चेतना प्रज्ञा भी इस समय उपस्थित रहती हैं। इस अवस्था में जीव परमात्मा के निकट सम्पर्क में रहता है। जिस प्रकार किसी स्त्री के मुख पर मलमल का झीना-सा घूँघट होने के कारण उसके पति को उसका मुख नहीं दिखायी देता, ठीक उसी प्रकार अज्ञानता का झीना-सा आवरण जीवात्मा को परमात्मा से अलग करता है। वेदान्ती इस अवस्था का गहन अध्ययन करते हैं। इसका गहन दार्शनिक महत्त्व है। यह आत्मा के अन्वेषण हेतु आधार प्रदान करती है। इस अवस्था में आप जगन्माता राजराजेश्वरी जो दैनिक जीवन में आगामी संघर्षों का सामना करने के लिए आपको शान्ति, नवीन मानसिक शक्ति अथवा शारीरिक बल प्रदान करती हैं, उनकी गोद में विश्राम करते हैं। गहन निद्रा में कृपालु माँ के अतुलनीय प्रेम तथा दया के बिना इस भूमण्डल पर (यहाँ अनेक कष्ट, रोग, उत्तरदायित्व, व्याकुलताएँ प्रतिक्षण आपको अपार कष्ट और पीड़ा दे रहे हैं) आपका जीवन असम्भव हो जाता। यदि आप एक रात भी गहरी नींद नहीं सो पाते हैं, तो आप कितना कष्ट,, विषाद, हताशा अथवा दुःख अनुभव करते हैं। कभी जब आप रात के समय सिनेमा का आनन्द लेने गये होंगे और ३ या ४ घण्टे की नींद खराब हो गयी होगी, तो ऐसा आपने कई बार अनुभव किया होगा।
ज्ञानदेव, भर्तृहरि तथा पतंजलि के समान महान योगी अक्सर मानसिक सम्प्रेषण (मन के द्वारा अन्यों के विचार पढ़ने की विधि) तथा विचारों के सम्प्रेषण द्वारा दूरस्थ व्यक्तियों को सन्देश भेजते थे और ग्रहण करते थे, इसे प्रथम टेलीग्राफ अथवा दूरसंचार सेवा माना जाता है। विचार अन्तरिक्ष में अद्भुत गति से जाते हैं। विचारों में गति होती है। इनमें भार, आकार, रूप तथा रंग होता है। इनमें अद्भुत शक्ति है।
यह संसार क्या है? यह हिरण्यगर्भ अथवा ईश्वर के विचार रूपों के भौतिकीकरण के सिवा कुछ नहीं है। जिस प्रकार विज्ञान में ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत् की लहरें हैं, उसी प्रकार योग में विचारों की लहरें हैं। प्रत्येक को अनजाने ही विचारों की लहरों का कम या अधिक अनुभव होता ही है। यदि आपको विचारों के स्पन्दनों की किंचित् भी समझ हो, यदि आप विचारों के नियन्त्रण की विधि जानते हों, यदि आप स्पष्ट, सुलझे हुए शक्तिशाली विचारों के निर्माण द्वारा लाभदायक विचारों को दूरस्थ व्यक्तियों तक सम्प्रेषित करने की विधि जानते हैं, तो आप इस विचार शक्ति को हजार गुना अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। विचारों के द्वारा अद्भुत कार्य भी होते हैं। एक गलत विचार बन्धन में डालता है और एक सही विचार मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए सही ढंग से सोचें और मोक्ष प्राप्त करें।
प्रिय बच्चो! मन की शक्तियों को समझ कर उनका साक्षात्कार करके अपने भीतर की शक्तियों को अनावृत करें। अपने नेत्र बन्द करें और सहजतापूर्वक धारणा करें। आप दूरस्थ विषयों को देख सकेंगे, दूरस्थ ध्वनियों को सुन सकेंगे, इस संसार ही नहीं वरन् अन्य ग्रहों को भी सन्देश भेज सकेंगे, अपने से हजारों मील दूर स्थित लोगों का उपचार कर सकेंगे तथा सुदूर स्थित जगहों पर तत्काल पहुँच सकेंगे। मन की शक्ति में विश्वास रखें। रुचि, अवधान, संकल्प-शक्ति, आस्था तथा धारणा से इच्छित फल प्राप्त होंगे। स्मरण रखें, मन का जन्म आत्मा की माया अर्थात् उसकी मोहिनी-शक्ति के द्वारा हुआ है।
ब्रह्माण्डीय दैवी मन विश्व का मन है। यह सम्पूर्ण वैयक्तिक मनों का योग है । ब्रह्माण्डीय मन हिरण्यगर्भ अथवा ईश्वर का मन है। मनुष्य का मन ब्रह्माण्डीय मन एक अंश मात्र हैं। अपने क्षुद्र मन को वैश्विक मन में विलीन करने और सर्वज्ञता प्राप्त करने तथा दैवी चेतना का अनुभव करना सीखें।
मन को सदा सन्तुलित रखें। यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। निस्सन्देह अभ्यास करना अत्यन्त कठिन है, लेकिन यदि आप धारणा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका अभ्यास करना ही होगा। सुख और दुःख में, गर्मी और सर्दी में, प्रशंसा और आलोचना में, आदर और अनादर में मन को सन्तुलित करना सच्चा ज्ञान है। इसके लिए अत्यधिक प्रयत्न की आवश्यकता है। यदि आप यह करने में सफल हो गये, तो आप संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन जायेंगे। आप श्रद्धा करने योग्य होंगे। चाहे आप चिथड़ों में लिपटे हों, चाहे आपके पास खाने के लिए कुछ भी न हो तो भी आप दुनियाँ में सबसे धनवान् व्यक्ति होंगे। चाहे आप शारीरिक रूप से दुर्बल हों, परन्तु आप सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। सांसारिक व्यक्ति तुच्छ वस्तुओं के लिए अपने मन का सन्तुलन खो देते हैं। वे शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं और अपना सन्तुलन खो बैठते हैं। जब कोई अपना सन्तुलन खो देता है, तो ऊर्जा नष्ट होती है। जो मन के सन्तुलन का विकास करना चाहते हैं, उन्हें विवेक का विकास करना ब्रह्मचर्य और धारणा का अभ्यास करना चाहिए। जो अपने वीर्य का नाश करते हैं शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। मन का नियन्त्रण तथा धारणा का अभ्यास अत्यन्त कठिन है सन्त तायुमानवार ने मन के नियन्त्रण पर अत्यन्त सुन्दर कविता लिखी है, उसका अनुवाद नीचे दिया जा रहा है :
आप एक पागल हाथी को नियन्त्रित कर सकते हैं।
आप भालू अथवा बाघ के मुख को बन्द कर सकते हैं।
आप शेर पर सवारी कर सकते हैं।
आप कोबरा नाग के साथ खेल सकते हैं।
रसायन विद्या द्वारा आप आजीविका कमा सकते हैं।
आप देवताओं को अनुचर बना सकते हैं।
आप चिरयुवा रह सकते हैं।
आप जल पर चल सकते हैं।
आप अग्नि के भीतर जीवित रह सकते हैं।
आप घर बैठे-बैठे ही सभी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन मन को नियन्त्रित करना तथा
इसके द्वारा शान्ति प्राप्त करना अत्यन्त दुर्लभ और कठिन है।
इन्द्रियाँ आपकी सच्ची शत्रु हैं। वे आपको बाहर खींच ले जाती है तथा आपकी मन की शान्ति को भंग कर देती हैं। उनका साथ न दें। उनको वश में करें। उन्हें रोकें। जिस प्रकार आप युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को पराजित करते हैं, उसी प्रकार इन्हें भी पराजित करें। यह कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है। इसके लिए दीर्घ काल तक धैर्यपूर्वक साधना की आवश्यकता है। इन्द्रियों पर नियन्त्रण ही वास्तव में मन पर नियन्त्रण हैं। सभी दस इन्द्रियों पर नियन्त्रण किया जाना चाहिए। उनको भूखा रख कर मार डालें। जो वे चाहती हैं, उन्हें वह कदापि न प्रदान करें। तब वे आपके आदेशों का सरलता से पालन करेंगी। सभी सांसारिक व्यक्ति हालाँकि वे पढ़े-लिखे हैं, उनके पास प्रचुर सम्पदा तथा न्यायिक और अधिशासी क्षमताएँ है, अपनी इन्द्रियों के दास होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप मांस भक्षण के आदी हैं, तो मांस भक्षण छह माह के लिए पूर्णतया त्यागने के लिए आपको इसी क्षण से जिह्वा पर नियन्त्रण करना प्रारम्भ कर देना चाहिए। तब आप ६ माह बाद मांस भक्षण पूर्णतया त्याग सकेंगे। आपको निरन्तर ऐसा अनुभव होगा कि आपने इस सर्वाधिक कष्ट देने वाली इन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर ली है, जो कुछ समय पूर्व आपसे विद्रोह करती थी।
सावधान, जागरूक और चौकन्ने तथा सतर्क बनें। अपने मन तथा उसके रूपान्तरों को देखें। प्रभु ईसामसीह कहते हैं- "देखो और प्रार्थना करो।" मन को देखना अन्तरावलोकन कहलाता है। करोड़ों में से एक व्यक्ति ही इस लाभदायक और आत्मोत्थानकारी अभ्यास को करता है। लोग सांसारिकता में निमग्र रहते हैं। वे पागलों की भाँति धन और स्त्री के पीछे भागते रहते हैं। उनके पास ईश्वर तथा उच्च आध्यात्मिक बातों के बारे में विचार करने का समय ही नहीं होता है। सूर्योदय होते ही मन पुनः अपनी खाने पीने, आनन्द उपभोग आदि की पुरानी ऐन्द्रिक लीकों की ओर दौड़ने लगता है। दिन बीत जाता है और इसी प्रकार सम्पूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है। न तो उनका नैतिक विकास होता है, न ही आध्यात्मिक विकास। जो नित्य अन्तरावलोकन करते हैं, वे अपने दोष ढूँढ़ सकते हैं तथा उन्हें अनुकूल विधियों द्वारा दूर कर सकते हैं और धीरे-धीरे मन पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी मानसिक कार्यशाला के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को प्रवेश नहीं करने देते हैं। वे निरन्तर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। नित्य आत्म-विश्लेषण तथा आत्म-निरीक्षण अन्य अनिवार्य अभ्यास है। इनको करने के द्वारा ही मात्र आप अपने दोषों को दूर कर सकेंगे और धारणा में शीघ्र आगे बढ़ सकेंगे। एक माली क्या करता है? वह नवजात पौधों को सावधानीपूर्वक देखता है, उनकी खतपतवार को नित्य हटाता है, उनके चारों ओर मजबूत बाड़ लगा देता है और नित्य सही समय पर उनको पानी देता है तथा इसी कारण उनकी अच्छी वृद्धि होती है और शीघ्र फल आते हैं। इसी प्रकार आपको अन्तरावलोकन तथा आत्म-विश्लेषण द्वारा अपने दोष ढूँढने चाहिए और अनुकूल विधियों द्वारा उनको निकाल फेंकना चाहिए। यदि एक विधि असफल हो जाये, तो आपको अन्य विधि अपनानी चाहिए। इस अभ्यास हेतु धैर्य, अध्यवसाय, जोंक भाँति दृढता, लौह सकल्प, सूक्ष्म बुद्धि तथा साहस की आवश्यकता है। लेकिन इससे प्राप्त होने वाला पुरस्कार अनमोल होगा। यह पुरस्कार अमरत्व परम शांति और अनन्त आनन्द है।
आपको मन को शान्त रखने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको अपनी योग की सीढ़ी पर प्रत्येक क्षण मन को शान्त बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि आपका मन बेचैन है, तो आप धारणा में किचित् भी प्रगति नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रथम और सर्वाधिक आवश्यक बात है कि आप सभी साधनों द्वारा मन की निश्चलता को प्राप्त करें। प्रातः काल शान्त ध्यान, कामनाओं का त्याग, अनुकूल आहार, इन्द्रियों का संयम तथा नित्य प्रति कम से कम एक घण्टे का मौन —ये सभी मन में शान्ति लायेंगे। सभी प्रकार के व्यर्थ के विचार, जंगली कल्पनाएँ, गलत भावनाएँ, उत्तरदायित्व, चिन्ताएँ, आकुलताएँ, भ्रामक विचार तथा सभी प्रकार के काल्पनिक भय ज्ञानाग्नि के द्वारा दूर किये जाने चाहिए। इनके उन्मूलन के पश्चात् ही आप शान्त मन प्राप्त करने की आशा कर सकते है। योग की नींव तभी अच्छी प्रकार से तथा वास्तव में डाली जायेगी,जब कि साधक में निश्चलता उच्चतम स्तर की होगी। मात्र एक शान्त मन सत्य को ग्रहण कर सकता है, ईश्वर के दर्शन कर सकता है और दैवी प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। यदि आपका मन शान्त होगा, तो आध्यात्मिक अनुभव स्थायी होंगे, अन्यथा वे आयेंगे और चले जायेंगे।
जैसे ही उन प्रातःकाल जागे, ईश्वर से प्रार्थना करें, उनके नाम का जप करें ४ से ६ बजे तक उन पर ध्यान करें। तत्पश्चात् निश्चय करें "आज मैं ब्रह्मचर्य का पालन करुँगा । आज मैं सत्य बोलूंगा। आज मैं किसी को आहत नहीं करूंगा। आज मैं अपने मन का संतुलन नहीं बिगड़ने दूंगा।" अपने मन को देखें। अपने संकल्प पर दृढ़रहें । आप निश्चय ही उस दिन सफल होंगे। तत्पश्चात् इस संकल्प को एक सप्ताह तक दोहरायें। इससे आपको शक्ति प्राप्त होगी। आपकी संकल्प-शक्ति का विकास होगा। तत्पश्चात् इस संकल्प को एक माह तक निरन्तर चलने दें। यहाँ तक कि यदि आपसे प्रारम्भ में भूल भी हो जाये, तो भी आपको अनावश्यक रूप से चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। भूलें आपकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। आप वही भूल दोबारा नहीं करेंगे। यदि आप सच्चे और लगनशील हैं, तो ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा-वृष्टि अवश्य करेंगे। ईश्वर आपको दैनिक जीवन के संग्राम में आने वाली कठिनाइयों में और परेशानियों का सामना करने हेतु शक्ति प्रदान करेंगे।
जिसने अपने मन को नियन्त्रित कर लिया है, वही वास्तव में स्वतन्त्र और प्रसन्न है। शारीरिक स्वतन्त्रता किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं है। यदि आप उबलते आवेगों तथा भावनाओं में आसानी से बह जायेंगे, यदि आप चित्तवृत्तियों तथा प्रलोभनों के फेर में होंगे, तो आप वास्तव में कैसे प्रसन्न रहेंगे। प्रिय बच्चे! आप बिना पतवार की नौका के समान होंगे। आप बृहत् समुद्र के बीच तिनके की भाँति इधर से उधर धकेले जाते रहेंगे। आप ५ मिनट के लिए हँसते हैं और ५ घण्टे तक रोते हैं। जब आप मन के आवेगों के बहाव में होंगे, तो पत्नी, पुत्र, मित्र, धन और शक्ति आपके लिए क्या कर सकते हैं? वह ही सच्चा नायक है, जिसने अपने मन को नियन्त्रित कर लिया है। एक कहावत है- "मन जीता, तो जग जीता।" मन पर विजय ही सच्ची विजय है। यही सच्ची स्वतन्त्रता है। कठोर संयम और स्व- आरोपित प्रतिबन्धों के द्वारा सभी कामनाएँ, विचार, आवेग, लोभ तथा वासनाएँ दूर हो जायेंगी। मात्र तभी आप मन को दासता से मुक्त हो सकेंगे। आपको मन को थोड़ा भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। मन एक शरारती बच्चा है। इसे कठोर प्रयत्नों द्वारा वश में करें। पूर्ण योगी बनें। धन आपको मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे बाजार में खरीदा जा सके। यह एक दुर्लभ, गुप्त खजाना है, जिसकी रखवाली पाँच फनों वाला नाग करता है। जब तक आप इस नाग को मार नहीं डालेंगे अथवा इसे पालतू नहीं बना लेंगे, आप इस खजाने को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यह खजाना है आध्यात्मिक सम्पत्ति, यही मुक्ति है, यही आनन्द है। नाग है आपका मन। इसके पाँच फन हैं आपकी पाँचों इन्द्रियाँ, जिनके द्वारा मन रूपी नाग कुफकारता है।
राजसिक मन सदैव नयी वस्तुओं की माँग करता है। इसे विभिन्नता चाहिए। इसे एकरसता से अरुचि है। इसे स्थान में परिवर्तन, आहार में परिवर्तन संक्षेप में कहें तो प्रत्येक चीज़ में परिवर्तन चाहिए। लेकिन आपको इसे एक चीज़ से चिपके रहने का प्रशिक्षण देना होगा। आपको एकरसता की शिकायत नहीं करनी चाहिए। आपमें धैर्य, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयत्न की आवश्यकता है। तभी आप योग में आगे बढ़ सकेंगे। जो सदैव नयी चीज की माँग करता है, वह योग के लिए पूर्ण अयोग्य है। आपको एक स्थान, एक आध्यात्मिक गुरु, एक विधि, योग के किसी एक प्रकार पर टिके रहना होगा। यह सकारात्मक सफलता का मार्ग है।
आपके भीतर ईश्वर-साक्षात्कार की प्रबल और सच्ची प्यास होनी चाहिए । तब सभी बाधाएँ दूर हो जायेगी। तब आपके लिए धारणा एकदम सरल होगी। मात्र उत्सुकतावश थोड़े समय के लिए भावनात्मक आवेगों अथवा सिद्धि प्राप्ति की आकांक्षा से वास्तविक परिणाम नहीं प्राप्त होंगे।
यदि आप असावधान है, यदि आप धारणा में अनियमित है, यदि आपका वैराग्य क्षीण हो गया है. यदि आप आलस्यवश कुछ दिनों के लिए अभ्यास छोड़ते. हैं, तो विरोधी बल आपको योग के मार्ग से दूर ले जायेंगे। आप असहाय हो जायेंग आपको वास्तविक ऊंचाई तक पहुँचना कठिन होगा। इसलिए धाराणा में नियमित रहें।
सदा उत्साहित और प्रसन्न रहे। हताशा और निराशा से दूर रहें । हताशा से बढ़ कर संक्रामक और कुछ नहीं है। हताश और निराश व्यक्ति मात्र अप्रिय और विकृत स्पन्दन ही चारों ओर फैलाते हैं। वे आनन्द, शान्ति और प्रेम का विकिरण कर ही नहीं सकते। इसलिए यदि आप हताश और निराश हो, तो अपने कमरे से कभी बाहर न आये, ऐसा न हो कि आप अपने चारों ओर संक्रमण फैला दें। अन्यों के लिए वरदान बन कर ही मात्र जिये। आनन्द, शान्ति और प्रेम का विकिरण करें। हताशा आपके अस्तित्व को खा जाती है और आपका विनाश कर देती है। यह वास्तव में प्लेग के समान मारक है। असफलता, गम्भीर अजीर्ण अथवा गर्म बहस, गलत विचारों अथवा गलत भावनाओं के कारण हताशा प्रकट होती है।
स्वयं को इस नकारात्मक भावना से दूर करें तथा स्वयं को परमात्मा के साथ एक कर लें। तब कोई भी बाह्य प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा। आप अभेद्य होंगे। जिस भगवान के नाम का कीर्तन, प्रार्थना, ॐ का नाद, प्राणायाम, खुली वायु मे तेजी से भ्रमण विपरीत गुणों के बारे में विचार जैसे आनन्द के भाव आदि पर विचार के द्वारा हताशा और निराशा की भावना को तत्क्षण दूर भगा दें। सभी स्थितियों में प्रसन्न रहने तथा अपने चारों ओर मात्र आनन्द विकिरित करने का प्रयत्न करें।
मेरे बच्चे तुम रोते क्यों हो? अपनी आँखों पर से पट्टी हटा दो और अब देखो आपके चारों ओर मात्र सत्य ही है। सभी मात्र प्रकाश और आनन्द हैं। अज्ञानता के अन्धकार ने आपकी आँखों को धुंधला कर दिया है। तत्क्षण इस अन्धकार को हटा दें। धारणा के नियमित अभ्यास द्वारा ज्ञान के अन्त: चक्षु का विकास कर नया चश्मा पहनें।
विचार ही एकमात्र कर्म का निर्धारण नहीं करते। कुछ बुद्धिमान पुरुष है, जो किसी वस्तु के समर्थन और विपक्ष में विचार करते हैं; लेकिन जब समय आता है, तो वे प्रलोभनों द्वारा प्रलोभित हो जाते हैं। वे गलत कार्य करते हैं और बाद में पश्चात्ताप करते हैं। यह वह भाव है, जो वास्तव में कर्म करने हेतु प्रेरित करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक परिकल्पना पर दबाव डालते हैं और कहते हैं कि वास्तव में परिकल्पना ही है, जो कि कर्मों का निर्धारण करती है। वे अपने दृष्टिकोण के समर्थन में निम्न उदाहरण देते हैं मान लीजिए कि २० फुट ऊँचे दो खम्भों के ऊपर एक फुट चौड़ा पटिया रखा हुआ है। जब आप इस पर चलना प्रारम्भ करते हैं, तो आप कल्पना करते हैं कि आप नीचे गिर जायेंगे और आप वास्तव में नीचे गिर जाते हैं; किन्तु जब यही पटिया भूमि पर रखा होगा, तो आप उस पर चल पायेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक सँकरी गली में से एक साइकिल पर सवार हो कर जा रहे हैं। आपको मार्ग में एक बहुत बड़ा पत्थर दिखायी देता है। आप कल्पना करते हैं कि आपकी साइकिल पत्थर से टकरा जायेगी और सच में आप साइकिल उस पत्थर की ओर दौड़ा देते हैं। अर्थात् यह परिकल्पना ही है जो कर्मों का निर्धारण करती है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक हैं, जो कहते हैं- "यह इच्छा शक्ति है जो कर्मों का निर्धारण करती है। इच्छा-शक्ति कुछ भी कर सकती है। इच्छा-शक्ति आत्मा की शक्ति है। " वेदान्ती इस बाद वाली धारणा को मानते हैं।
अब हम धारणा के विषय पर वापस आ जाते हैं। विचारों के रूपों द्वारा मन में जो लहरें निर्मित होती हैं, उन्हें वृत्तियाँ कहते हैं। इन लहरों को स्थिर करना अथवा रोकना चाहिए। तभी आप आत्म-साक्षात्कार कर सकेंगे। अच्छी तरह प्रशिक्षित मन अपने संकल्प के अनुसार शरीर के बाहर अथवा भीतर किसी भी विषय पर एकाग्र किया जा सकता है। धारणा का अभ्यास प्रारम्भ में थोड़ा अरुचिकर प्रतीत होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात् यह अत्यधिक आनन्द प्रदान करता है, किन्तु इसके लिए धैर्य तथा अध्यवसाय और नियमितता आवश्यक है। हिन्दू शास्त्रों में मन की तुलना झील अथवा सागर से की गयी है। मन से उत्पन्न होने वाली लहरों की तुलना समुद्र की लहरों से की गयी है। जब समुद्र की सतह की सभी लहरें पूर्णतः शान्त हो जायें और स्थिर हो जायें, उस समय ही आप समुद्र के पानी में अपनी परछाई स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए आप आत्मा का, उस ज्योतियों की ज्योति का साक्षात्कार मात्र तभी कर सकते हैं, जब कि मन रूपी झील में सभी विचार लहरें स्थिर हो जायें।
यदि आप धारणा के अभ्यास में रुचि लें, यदि आपका एक निश्चित उद्देश्य हो तो धारणा के अभ्यास में आपकी प्रशंसनीय प्रगति होगी। नवाभ्यासियों की अभ्यास में बड़ी रुचि रहती है, किन्तु जब उनको कुछ अनुभव जैसे चमकीला प्रकाश दिखाद देना, दैवी नाद सुनायी देना, विशेष सुगन्धि का अनुभव होना आदि अनुभव होते है, तो स्वयं को एक पूर्ण योगी समझने लगते हैं।
कुछ लोग मात्र सुखकर अथवा रुचिकर विषयों पर ही धारणा कर सकते हैं। यदि वे अरुचिकर विषयों में भी रुचि उत्पन्न कर सकें, तो वे अरुचिकर वस्तुओं पर भी तो मन एकाग्र हो जाता है और आपको भीतर से आनन्द प्राप्त होता है। यदि ध्यान और धारणा से प्राप्त होने वाले आनन्द से तुलना की जाये, तो समस्त संसार के सुख कुछ भी नहीं है। किसी भी मूल्य पर धारणा का अभ्यास न छोड़े। आगे बढ़े। धैर्य, अध्यवसाय उत्साह, हठ तथा प्रयास जारी रखें। आप निश्चय ही आगे बढ़ेंगे। निराश न हो। श्री शंकराचार्य जी ने अपनी छान्दोग्य उपनिषद् की व्याख्या में लिखा है- "मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण करे और मन की धारणा करे (अध्याय ७-२१-१)। गम्भीर अन्तरावलोकन द्वारा उन विभिन्न बाधाओं को ढूंढ निकालें, जो आपकी धारणा में बाधक है और उन्हें प्रयत्न द्वारा एक-एक करके दूर करें। नये विचारों (संकल्पों) और कामनाओं (वासनाओं) को जन्म न लेने दें। विवेक, जिज्ञासा, धारणा तथा ध्यान द्वारा उन्हें कलिकावस्था में ही नष्ट कर दें।
प्रत्येक व्यक्ति जब कोई पुस्तक पढ़ता है या टेनिस खेलता है अथवा किसी भी प्रकार का कार्य करता है, तो एक विशेष सीमा तक धारणा करता ही है। लेकिन आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए धारणा का अत्यधिक उच्च स्तर तक विकसित होना आवश्यक है। मन एक बेलगाम बन्दर के समान है। इसके पास एक समय में एक ही विषय पर ध्यान देने की शक्ति है, लेकिन यह अत्यन्त शीघ्रता से तथा अद्भुत गति से एक विषय से दूसरे विषय पर जा सकता है। वास्तव में कुछ ने देखा कि यह एक समय में कई बातों को ग्रहण कर सकता है। लेकिन पश्चिम तथा पूर्व के कुछ श्रेष्ठ दार्शनिकों और मनीषियों ने पाया कि एक विचार वाला सिद्धान्त अधिक सही है। ऐसा ही कई व्यक्तियों को स्वयं के अनुभव से भी ज्ञात हुआ है। मन सदैव बेचैन रहता है। यह रजोगुण तथा वासनाओं के कारण होता है। भौतिक विषयों में सफलता हेतु अवधान अनिवार्य है। एक व्यक्ति जिसके पास प्रशंसनीय स्तर का अवधान है, उसके पास अपेक्षाकृत अधिक अर्जन-क्षमता होती है तथा वह कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। मुझे यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि योग के विद्यार्थी को उसके धारणा में प्रयत्न का फल अवश्य ही प्राप्त होगा ?
जब आप कोई पुस्तक पढ़ें, तो अपना पूरा मन हाथ में लिये गये विषय पर लगायें। मन को किसी भी बाह्य विषय को देखने अथवा किसी भी ध्वनि को सुनने न दें। मन की बिखरी हुई किरणों को एकत्रित कीजिए। अवधान की शक्ति का विकास कीजिए। अवधान जैसा कि मैंने प्रारम्भ में भी कहा है कि इसकी धारणा में कोई अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, वरन् धारणा वास्तव में अवधान के विस्तृत क्षेत्र को छोटा करना है। यह प्रशिक्षित संकल्प शक्ति का एक प्रतीक है। एक दृढ व्यक्तित्व के स्वामी पुरुष की धारणा उत्तम होती है।
उन कार्यों पर अवधान का अभ्यास करें, जिनको करने में आपको उनकी अप्रियता के कारण संकोच का अनुभव होता है। अरुचिकर विषयों तथा विचारों पर रुचि लेने का प्रयत्न करें। उनको अपने मन के सामने रखें। धीरे-धीरे रुचि प्रकट होगी। अनेक मानसिक दुर्बलताएँ नष्ट हो जायेंगी। मन दृढ और अधिक दृढतर होता जायेगा। वह शक्ति जहाँ कोई भी चीज मन पर आघात करती है, वह सामान्यतया उस अनुपात में होता है, जिस स्तर का अवधान इस पर डाला जाता है। इसके अतिरिक्त ध्यान स्मरण शक्ति की महान कला है और अकर्मण्य लोगों की स्मरण शक्ति दुर्बल होती है।
जब आप ताश अथवा शतरंज खेलते हैं, तो आपकी अच्छी धारणा होती है, लेकिन तब आपके मन में शुद्ध एवं दैवी विचार नहीं होते। इस समय मन तत्त्व एक अवांछनीय प्रकृति के होते हैं। जब आपका मन अशुद्ध विचारों से भरा होगा, तो आप दैवी रोमांच, भावोत्कर्ष तथा मन के उत्थान का अनुभव नहीं कर पायेंगे। प्रत्येक विषय का अपना मानसिक संयोजन होता है। आपको मन को उत्कृष्ट तथा आध्यात्मिक विचारों से भरना चाहिए, तभी सभी सांसारिक विचारों से आपके मन का शुद्धिकरण हो सकेगा। श्री कृष्ण, भगवान् बुद्ध अथवा प्रभु ईसामसीह का चित्र उत्कृष्ट आत्मोत्थानकारी विचारों से संयुक्त रहता है, जब कि शतरंज, ताश, द्यूत कपट आदि से संयुक्त रहते है।
छाया - त्राटक से दृश्य अथवा अदृश्य विषयों की प्राप्ति होती है। इसके अभ्यास से मनुष्य निस्सन्देह शुद्ध बन जाता है। छाया उन सभी प्रश्नों के उत्तर देती है, जो आप जानना चाहते हैं। वह योगाभ्यासी जो अपनी छाया को आकाश में देखने में सक्षम होता है। वह जान सकता है कि उसके हाथ में लिये गये कार्यों में उसे सफलता मिलेगी या नहीं। जिन योगियों ने धारणा के लाभों का साक्षात्कार किया है, उन्होंने कहा है-"सूर्य के प्रकाश में अपनी छाया को अपलक देखिए, चाहे आपको यह एक ही क्षण के लिए आकाश में दिखायी दे। उस समय आप ईश्वर को तत्क्षण आकाश में देख लेते हैं।" जो नित्य इस आकाश में अपनी छाया को देखता है, वह दीर्घायु प्राप्त करता है। उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जब छाया पूर्णतः स्पष्ट रूप से दिखायी दे, तो योगाभ्यासी को विजय और सफलता मिलती है। वह प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और सर्वत्र विचरण कर सकता है। यह अभ्यास अत्यन्त सरल है। व्यक्ति को इस अभ्यास में अत्यन्त शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। कुछ लोगों को एक या दो सप्ताह में ही परिणाम होने लगते हैं। अब सूर्योदय हो, तो इस प्रकार खड़े हो कि आपकी छाया भूमि पर पड़े और आप इसे बिना किसी कठिनाई के देख सके। तत्पश्चात् आप कुछ देर तक अपनी गर्दन पर अपलक दृष्टि जमायें । इसके बाद आकाश की ओर देखें। यदि आप आकाश में अपनी छाया का पूर्ण प्रतिबिम्ब देख पाते हैं, तो यह अत्यन्त शुभ है। यह आपके प्रश्नों के उत्तर देगी। यदि आपको छाया न दिखायी दे तो तब तक अभ्यास करते रहे, जब तक आप इसे देख न लें। आप इसका अभ्यास चांदनी रात में भी कर सकते हैं।
कुछ लोग जब उनके शरीर का कोई अंग किसी रोग से पीड़ित होता है, तो वे अत्यधिक दर्द अथवा कष्ट का अनुभव करते हैं। इसका कारण ढूँढ़ना अधिक कठिन नहीं है। वास्तव में वे सदैव रोग के बारे में विचार करते रहते हैं और शरीर के रोग प्रभावित अंग से किस प्रकार मन को दूर ले जा कर किसी अन्य विषय पर कैसे लगाया जाये, इसकी विधि नहीं जानते। कुछ लोग अन्यों की तुलना में कम दर्द का अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को मन को रोग के स्थान से किस प्रकार हटाया जाये, इसका ज्ञान होता है। जब भी आपके शरीर में दर्द का अनुभव हो, तो अपने इष्टदेवता पर धारणा करें अथवा किसी दार्शनिक पुस्तक का अध्ययन करें। दर्द समाप्त हो जायेगा।
धारणा स्थिर मानसिक क्रिया-विधि है। इसके लिए मन को भीतर की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। यह पेशीय गतिविधि नहीं है। इसमें मस्तिष्क पर कोई अनावश्यक तनाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको मन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए।
एक आरामदायक आसन में बैठ जाये। शरीर की सभी मांसपेशियों को शिथिल कर दें। शरीर में किसी भी प्रकार की पेशीय, भावनात्मक, नाड़ीय अथवा मानसिक कार्य शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। मन को स्थिर करें। उमड़ते हुए विचारों को शान्त करें। आवेगों को शान्त करें] विचारों की क्रिया पर रोक लगा दें। अवांछनीय विचारों पर ध्यान न दें। मन को सुझाव दें- ''मैं कोई चिन्ता नहीं करता, चाहे वे हों या नहीं।" अर्थात् निरपेक्ष रहें। मानसिक कार्यशाला के भीतर अवांछनीय विचार शीघ्र शान्त हो जायेंगे कोई परेशानी नहीं देंगे। यह मानसिक संयम का रहस्य है। धारणा में विकास धीरे-धीरे परिलक्षित होगा। किसी भी मूल्य पर विचलित न हों। अपने अभ्यास में नियमित रहें। एक दिन के लिए भी अभ्यास न छोड़ें। प्रभु यीशु कहते हैं-"स्वयं को रिक्त कर दो और मैं तुम्हें भर दूँगा।" जब आपको धारणा की कुछ शक्ति प्राप्त हो जायेगी, तभी आप इन विचारों को रिक्त करने की क्रिया विधि को कर सकेंगे। स्वयं को सदैव सकारात्मक स्थिति में रखें। जब आप किसी कार्य के अंश पर धारणा करना चाहें, तो इसे अत्यन्त ध्यान से करें। आप अपने समस्त संकल्पों तथा कल्पनाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। कल्पना धारणा में सहायता भी करती है।
अत्यधिक शारीरिक श्रम, अत्यधिक वार्तालाप, अत्यधिक भोजन, स्त्रियों तथा अनावश्यक लोगों से अत्यधिक घुलना-मिलना-धारणा का अभ्यास करने वालों को उपर्युक्त सभी बार्तो को त्याग देना चाहिए। आप जो भी कार्य करें, पूर्ण एकाग्रता के साथ करें। काम को पूरा होने से पहले बीच में कभी भी न छोड़ें।
ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, आवश्यकताओं तथा गतिविधियों में कमी, विषयों का त्याग, एकान्त-वास, मौन, इन्द्रियों का संयम, काम और लोभ का उन्मूलन तथा क्रोध पर नियन्त्रण करें। अवांछनीय लोगों की संगत, समाचारपत्र पठन एवं सिनेमा देखना छोड़ दें। ऐसा करने से धारणा की शक्ति में वृद्धि होती है।
यदि धारणा के समय आपका मन भागता है, तो भी आप चिन्ता न करें, इसे भागने दें। इसे धीरे से धारणा के विषय पर वापस ले कर आयें। प्रारम्भ में शायद यह ५० बार भागेगा दो वर्ष के अभ्यास के पश्चात् यह संख्या घट कर २० हो जायेगी, अगले तीन वर्षों के निरन्तर एवं दृढ़तापूर्ण अभ्यास के पश्चात् यह संख्या घट कर शून्य हो जायेगी। मन तब दैवी चेतना पर पूर्णतया केन्द्रित हो जायेगा। तब आप यदि इसे बाहर खींचना भी चाहेंगे, तो भी यह बाहर नहीं आयेगा। जिन्होंने मन के ऊपर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त किया है, यह उनका व्यक्तिगत अनुभव है।
अर्जुन का ध्यान अद्भुत था। उसने द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखी थी। एक बार की घटना है। नीचे एक जल से भरा बर्तन रख कर उसके ठीक ऊपर एक खम्भे से बाँध कर एक मृत चिड़िया को इस प्रकार लटकाया गया कि उसका प्रतिबिम्ब जल के बर्तन में पड़े और इस समय अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या को सिद्ध करने के लिए कहा गया। उसे इस चिड़िया के प्रतिबिम्ब को जल में देख कर असली चिड़िया की दाहिनी आँख पर निशाना लगाना था, अर्जुन ने उसका प्रतिबिम्ब देखा और चिड़िया की आँख पर निशाना लगाया। इस कला का बहुत कम लोगों को ज्ञान था।
नेपोलियन का भी ध्यान अद्भुत था। ऐसा कहा जाता है कि उसका अपने विचारों पर पूर्ण नियन्त्रण था। वह अपने मस्तिष्क के कोष्ठक में से एक विचार को खींच सकता था और उसी एक विचार पर जितनी देर तक वह चाहता, लीन रहता तथा फिर उसे वापस मस्तिष्क के कोष्ठक में वापस पहुँचा सकता था। उसके पास एक विशिष्ट मस्तिष्क था, जिसमें विशिष्ट कोष्ठक थे।
जब आप बड़ी रुचि से कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो आप अपना नाम ले कर पुकारने वाले व्यक्ति की आवाज भी नहीं सुन पाते। आपको अपने पास मेज पर रखे हुए फूलों के गुलदाने में से आती हुई सुगन्धि का भी अनुभव नहीं होता। यही धारणा है। यह चित्त की एकाग्रता है। मन इसमें मात्र एक ही वस्तु पर केन्द्रित रहता है। जब आप ईश्वर अथवा आत्मा के बारे में विचार करते हैं, तो आपके ध्यान की भी ऐसी ही गहराई और तीव्रता होनी चाहिए) सांसारिक वस्तुओं पर मन की धारणा करना सरल है, क्योंकि आदत के कारण मन स्वाभाविक रूप से उनमें अत्यधिक रुचि लेता है। मस्तिष्क में स्वयं ही लीकें कटी हुई हैं। आपको मन को बार-बार ईश्वर पर लगा कर नयी लीकें काटनी होंगी। कुछ समय पश्चात् मन बाह्य विषयों की ओर नहीं भागेगा, क्योंकि इसे भीतर ही आनन्द का अनुभव होने लगेगा।
कुछ पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों ने देखा - "वह मन जो निरुद्देश्य रूप से इधर-उधर भटकता है, मात्र धारणा के अभ्यास से एक सीमित घेरे में घूमने योग्य बनाया जा सकता है। इसे एक बिन्दु मात्र पर टिकाया नहीं जा सकता। यदि यह एक बिन्दु पर लगाया जा सकता, तो वहाँ मन का निरोध हो जाता। तब मन की मृत्यु हो जाती है। जब वहाँ मन का निरोध होगा, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।" लेकिन यह सही नहीं है। मन का पूर्ण नियन्त्रण सभी प्राप्त होगा, जब सभी विचारों की समस्त लहरों का सम्पूर्ण उन्मूलन हो जायेगा।। योगी इस मन की एकाग्रचित्तता के द्वारा अद्भुत कार्य करते हैं। योगी को मन की एकाग्रचित्तता के द्वारा उत्पन्न सर्वत्र प्रवेश करने वाले तीव्र प्रकाश की सहायता से आत्मा के छुपे खजाने का ज्ञान हो जाता है। एकाग्रता प्राप्त करने के पश्चात् पूर्ण निरोध अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। इस अवस्था में सभी रूपान्तर पूर्णतया शान्त हो जायेंगे। मन बिलकुल रिक्त हो जायेगा। तत्पश्चात् योगी स्वयं को उस परम पुरुष अथवा आत्मा (जिसके द्वारा मन स्वयं अपना प्रकाश लेता है) से एक कर रिक्त मन को भी नष्ट करता है। तब वह सर्वज्ञता अथवा कैवल्य प्राप्त करता है। ये विषय हमारे पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों के लिए ग्रीक अथवा लैटिन भाषा के समान हैं। वे अज्ञानता में घिरे हुए हैं। उनको इस सम्पूर्ण जगत् के साक्षी पुरुष का कोई विचार ही नहीं होता है।
मनुष्य एक जटिल सामाजिक प्राणी है। वह एक जैविक प्राणी भी है और इसी कारण उसे किसी विशेष शरीर विज्ञान के कार्यों जैसे रक्त का परिसंचरण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन द्वारा निश्चित रूप से पहचाना जाता है। वह किन्हीं विशेष मनोवैज्ञानिक कार्यों जैसे विचार करना, देखना, स्मरण शक्ति, कल्पना आदि द्वारा निश्चित रूप से पहचाना जाता है। वह विचार करता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, अनुभव करता है। दार्शनिक रूप से कहा जाता है कि वह ईश्वर का प्रतिबिम्ब ही नहीं, वरन् स्वयं ईश्वर है। उसने निषिद्ध वृक्ष के फल को चख कर अपनी दैवी गरिमा खो दी है। मन के संयम तथा धारणा के अभ्यास द्वारा वह अपनी दिव्यता पुनः प्राप्त कर सकता है।
९. योग - प्रश्नोत्तरी
प्रश्न : व्यक्ति को किस पर धारणा करनी चाहिए?
उत्तर : प्रारम्भ में किसी स्थूल रूप, भगवान् कृष्ण के मुरलीधर स्वरूप अथवा भगवान् विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप जिसमें वे अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हैं।
प्रश्न: एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैं दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब के भ्रूमध्य-स्थान पर त्राटक करूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ?
उत्तर : हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। यह धारणा का एक तरीका है। लेकिन एक विधि से चिपके रहें। जैसे यदि भगवान् राम के चित्र पर धारणा करते हैं, तो मात्र इसी पर करते रहें। यदि आप उनके दैवी रूप पर धारणा करेंगे तथा उनके गुणों पर ध्यान करेंगे, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी।
प्रश्न : लोग शालग्राम पर धारणा क्यों करते हैं?
उत्तर : क्योंकि इसमें धारणा को सरलतापूर्वक प्रेरित करने की शक्ति है।
प्रश्न: मैं त्रिकुटी, ॐ तथा ध्वनि के ऊपर त्राटक करता हूँ। क्या मैं अपनी धारणा सही कर रहा हूँ?
उत्तर: आप सही हैं। ॐ के साथ-साथ पवित्रता, सत्, चित्, आनन्द पूर्णता आदि के विचार भी संयुक्त कर दें। अनुभव करें कि आप सर्वव्यापक चेतना है। इस प्रकार का भाव आवश्यक है।
प्रश्न: मन की गहन धारणा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ?
उत्तर: मानसिक वैराग्य का विकास कीजिए अभ्यास के समय में वृद्धि लोगों के साथ न मिले तीन घण्टे का मौन रखें । रात्रि में दूध और फल लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मन की धारणा होगी।
प्रश्न : शिष्य को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। अक्सर वह अपने गुरु के सम्पर्क में रहना चाहता है। यही कारण है कि मैं आपको सदा परेशान करता रहता। क्या मैं अब यह जान सकता हूँ कि धारणा की शक्ति कैसे बढ़ सकती है?
उत्तर : आप अक्सर मुझे पत्र लिख सकते हैं। परेशानियाँ मन से सम्बद्ध होती है। वह आत्मा जो मन से परे होती है, जो उसमें स्थित रहते हैं, उनके लिए सदैव शान्ति रहती है। जो आत्मा में निवास करते हैं, उन्हें परेशानियाँ, कठिनाइयाँ तथा दुःख स्पर्श ही नहीं कर सकते। अपनी आवश्यकताओं तथा कामनाओं को कम करना, नित्य दो घण्टे मौन रखना, नित्य एकान्त कमरे में एक या दो घण्टे अकेले रहना, प्राणायाम का अभ्यास प्रार्थना सध्या तथा रात्रि में ध्यान की बैठकों में वृद्धि तथा विचार आदि करने से धारणा में वृद्धि होती है।
प्रश्न: जप से भी धारणा प्राप्त होती है?
उत्तर: हाँ। मानसिक जप करें।
प्रश्न : जब मैं त्रिकुटी पर धारणा करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सिरदर्द होता है। क्या इसका कोई उपचार है?
उत्तर : मन के साथ संघर्ष न करें। जब आप धारणा करें, हिंसात्मक प्रयास न करें। सभी नाड़ियों, पेशियों तथा मस्तिष्क को शिथिल कर दे। सहज रूप से हल्की धारणा करें। इससे अनावश्यक तनाव तथा उसके कारण होने वाला सिरदर्द दूर हो जायेगा।
प्रश्न: अभी भी मन भटकता है और प्रकाश दुर्बल है। धारणा के प्रयास कभी-कभी सफल रहते हैं, लेकिन अक्सर ये निराशा में समाप्त होते हैं। मन का शुद्धिकरण सरल नहीं है। इस हेतु आप क्या सुझाव देते हैं?
उत्तर: आपका वैराग्य प्रबल नहीं है। वैराग्य का विकास करें। प्रबल साधना करें। ध्यान के समय को तीन घण्टे तक बढ़ायें। अपनी गतिविधियाँ कम करें। ऋषिकेश अथवा उत्तरकाशी में तीन माह के एकान्त वास के लिए जायें। पूरे तीन माह तक मौन धारण करें। आपको अद्भुत धारणा और ध्यान प्राप्त होगा।
प्रश्न: वह योगी जो अपने शिष्य के ऊपर शक्ति संचार करता है, अपने शिष्य को सभी प्रकार की साधनाएँ त्यागने के लिए क्यों कहता है ?
उत्तर: उसके भीतर प्रबल आस्था का विकास करने तथा मार्ग में स्थिरता और योग के एक रूप में एकाग्रचित्तता अथवा सम्पूर्ण मन के विकास करने के लिए)
प्रश्न: मैं नित्य दो घण्टे जप करता हूँ तथा आधे घण्टे तक प्राणायाम करता हूँ। क्या मुझे दो अथवा तीन वर्षों में एकाग्रता तथा तन्मयता प्राप्त होगी?
उत्तर: हाँ। यदि आप अपनी साधना में शुद्ध और गम्भीर होंगे, तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी।
अध्याय २
धारणा का अभ्यास
१. अवधान
आपके भीतर धारणा के प्रति अच्छी रुचि होनी चाहिए। मात्र तभी आपका सम्पूर्ण अवधान उस विषय की ओर निर्दिष्ट होगा, जिस पर आप धारणा करना चाहते हैं। जब तक अभ्यासी द्वारा प्रशंसनीय स्तर की रुचि तथा अवधान नहीं प्रदर्शित किया जायेगा, तब तक किसी प्रकार की सच्ची धारणा नहीं हो सकती। इसलिए इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है, आपको यह जानना आवश्यक है।
अवधान मन को स्थिर करने का प्रयास है। यह चुने हुए विषय पर चेतना को केन्द्रित करना है। अवधान के द्वारा आप अपनी मानसिक क्षमताओं तथा योग्यताओं का विकास कर सकते हैं। जहाँ अवधान होगा, वहाँ धारणा भी होगी। अवधान का अर्जन धीरे-धीरे करना चाहिए। यह कोई विशेष विधि नहीं है। यह इसके एक पहलू में सम्पूर्ण मानसिक क्रिया विधि है।
देखने में सदैव अवधान सम्मिलित है। देखना अर्थात् अवधान करना। अवधान के द्वारा आपको विषयों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। जिस विषय की ओर अवधान निर्दिष्ट होता है, उसी के ऊपर सम्पूर्ण ऊर्जा केन्द्रित होती है और आपको उसकी पूर्ण और सम्पूर्ण सूचना प्राप्त होती है। अवधान में मन की बिखरी हुई समस्त किरणें एकत्रित होती है। अवधान में प्रयास अथवा संघर्ष होता है। अवधान के द्वारा किसी भी वस्तु का गहन प्रभाव पड़ता है। यदि आपका अवधान अच्छा है, तो आप हाथ में लिये गये कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। एक अवधान सम्पन्न व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। वह बहुत ही जागरूक और सावधान होता है। वह नम्र और सतर्क होता है।
अवधान धारणा में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह संकल्प का आधार है। जब अन्तरावलोकन के उद्देश्य से इसे अन्तर जगत् की ओर उचित प्रकार से निर्देशित किया जाता है, तो यह मन को विश्लेषित करता है और आपके लिए अनेक चौकाने बाले तथ्यों को प्रकाशित करता है।
अवधान चेतना का केन्द्रीकरण है। अवधान धारणा में एक सजग भूमिका निभाता है। यह प्रशिक्षित संकल्प का एक प्रतीक है। यह दृढ़ मानसिकता के व्यक्तियों में पाया जाता है। यह एक दुर्लभ योग्यता है। ब्रह्मचर्य इस शक्ति का अद्भुत ढंग से विकास करता है। वह योगी जिसके पास यह गुण होता है, वह अपने मन को किसी भी अरुचिकर विषय पर भी बहुत देर तक एकाग्र कर सकता है। मन जिस विषय को पसन्द करता हो, उस पर इसे एकाग्र करना सरल है। दृढ़ अभ्यास के द्वारा अवधान का अर्जन और विकास सम्भव है। सभी महान् व्यक्ति अवधान के द्वारा ही ऊपर उठे ।
आप जिस समय जो कार्य कर रहे हों, अपना पूरा अवधान उसी कार्य में लगायें। उन अरुचिकर कार्यों में अपना अवधान लगायें, जिनको करने में आपको उनकी अप्रियता के कारण संकोच होता था। अरुचिकर विषयों तथा विचारों में रुचि लें। उन्हें अपने मन के सामने रखें। धीरे-धीरे रुचि प्रकट होगी। अनेक मानसिक दुर्बलताएँ नष्ट हो जायेंगी। मन दृढ़ और दृढ़तर होता जायेगा।
वह बल जिसके द्वारा कोई भी वस्तु मन पर आघात करती है, उस स्तर पर निर्भर करता है जिस स्तर का अवधान उस पर डाला जा रहा है। स्मरण की महान् कला अवधान है। अकर्मण्य व्यक्तियों की स्मरण शक्ति दुर्बल होती है।
मानव-मन के पास एक समय में एक ही विषय पर ध्यान देने की शक्ति है, हालाँकि यह अत्यन्त शीघ्रता से इतनी अद्भुत गति से एक विषय से दूसरे विषय पर जा सकता है कि वास्तव में कुछ ने देखा कि यह एक समय में कई बातों को ग्रहण कर सकता हैं। लेकिन पश्चिम तथा पूर्व के कुछ श्रेष्ठ दार्शनिकों और मनीषियों ने पाया कि एक विचार वाला सिद्धान्त अधिक सही है। यह व्यक्तियों के अनुभव से भी सहमत है।
यदि आप मानसिक कार्यों अथवा गतिविधियों का सावधानीपूर्वक अन्वेषण करें, किसी एक विधि को अवधान नहीं कहा जा सकता है। अवधान को एक अलग कार्य की भाँति अलग करना सम्भव है। आप किसी बात को ग्रहण करते हैं, इसलिए उसके प्रति चैतन्य रहते हैं।
चेतना की प्रत्येक स्थिति से अवधान संयुक्त है और यह चेतना के प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित है। एक सजग विद्यार्थी आध्यात्मिक पथ में श्रुतियों का प्रभावशाली ढंग से श्रवण कर सकता है। सेना का अधिकारी कहता है सावधान! और सैनिक अपनी बन्दूक ले कर अपने शत्रुओं पर आक्रमण हेतु तैयार हो जाता है। मात्र एक सतर्क सैनिक ही अपना निशाना लगा सकता है। अवधान के बिना कोई व्यक्ति भौतिक अथवा आध्यात्मिक उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है।
ऐसे कई योगी हैं जो आठ या दस अथवा सौ कार्य एक साथ कर सकते हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है। इसका सम्पूर्ण रहस्य इस बात में सन्निहित है कि उन्होंने अपने अवधान का प्रशंसनीय स्तर तक विकास कर लिया है। जगत् के सभी महान् व्यक्तियों में यह योग्यता विभिन्न स्तर तक विकसित होती है।
अवधान दो प्रकार का होता है—बाह्य अवधान और अन्तर अवधान। जब अवधान बाह्य विषय की ओर निर्दिष्ट होता है, तो इसे बाह्य अवधान कहते हैं। जब इसे मन के भीतर मानसिक विचारों और विषयों पर निर्देशित किया जाता है, तो यह अन्तर अवधान कहलाता है।
अवधान अन्य दो प्रकार का भी होता है। ऐच्छिक अवधान और अनैच्छिक अवधान। जब संकल्प करके प्रयास द्वारा अवधान कुछ बाह्य विषयों की ओर निर्दिष्ट किया जाता है, तो यह ऐच्छिक अवधान कहलाता है। जब आप इसकी अथवा उसकी ओर ध्यान देने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यह ऐच्छिक अवधान कहलाता है। इसमें मनुष्य समझता है कि वह क्यों देखता है तथा इसमें कुछ निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य सम्मिलित होता है। ऐच्छिक अवधान हेतु प्रयत्न, संकल्प, निर्णय तथा थोड़ा मानसिक प्रशिक्षण आवश्यक है। अभ्यास तथा अध्यवसाय द्वारा इसमें वृद्धि की जा सकती है। अवधान के अभ्यास से प्राप्त होने वाले लाभ अगण्य हैं। अनैच्छिक अवधान अत्यन्त सामान्य है। इस हेतु किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। इसमें इच्छा का कोई प्रयत्न नहीं होता, यह विषय का सौन्दर्य अथवा आकर्षण देख कर प्रेरित होता है। इस अवधान में व्यक्ति बिना यह जाने कि क्यों और किसी निर्देश के अनुभव के बिना देखते हैं। छोटे बच्चों में अनैच्छिक अवधान की शक्ति बड़े लोगों की तुलना में बहुत अधिक होती है।
यदि एक व्यक्ति का ध्यान नहीं है, तो वह एकाग्र नहीं होता। यदि वह किसी बात पर ध्यान देता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह एकाग्र है। उद्देश्य, आशा, अपेक्षा, कामना, विश्वास, आकांक्षा, ज्ञान, लक्ष्य तथा आवश्यकताएँ अवधान हेतु निर्णायक होती हैं। आपको सावधानीपूर्वक अवधान के स्तर, अवधि, सीमा, रूपों, उतार-चढ़ाव तथा विचलनों को देखना चाहिए।
यदि कोई विषय अत्यधिक सुखदायक है, तो वहाँ गहन अवधान होता है। आपको रुचि उत्पन्न करनी होगी। तभी विषय पर अवधान होगा। यदि अवधान कम हो जाये, तो अपना अवधान किसी अन्य सुखकर विषय पर ले जायें। धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण के द्वारा आप रुचि उत्पन्न करके मन को किसी अरुचिपूर्ण विषय की ओर भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। तभी आपका संकल्प दृढ़ होगा।
यदि आप ध्यान से देखें, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न विषय पर जाता है। यह कभी एक विषय पर होता है, कभी दूसरे पर। जब भौतिक स्थितियाँ स्थिर होती हैं, तो इसे अवधान का विचलनीकरण कहते हैं। अवधान परिवर्तित हो रहा है। विषय स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं; लेकिन इनका अवधान करने वाले व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि मन को अधिक लम्बे समय तक अवधान करने हेतु प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। यह एकरसता से ऊब जाता है और किसी सुखकर विषय की ओर भागना चाहता है। आप कह सकते है कि मैं एक ही बात पर ध्यान दे सकता हूँ। लेकिन आप कुछ समय बाद देखेंगे कि हालाँकि आप बहुत अधिक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह अचानक किसी अन्य विषय को देखने लगता है। यह अवधान का विचलन है।
रुचि अवधान में वृद्धि करती है। मन को किसी अरुचिकर विषय पर लगाना कठिन है। जब कोई व्याख्याता पढ़ाता है और विषय अव्यावहारिक और तात्त्विक है, तो कई लोग चुपचाप कक्ष को छोड़ कर चले जाते हैं; क्योंकि वे उस विषय को नहीं ग्रहण कर पाते जो रुचिकर नहीं है। लेकिन वही व्याख्याता यदि गाना गाता है और अच्छी कहानी सुनाता है, तो सभी लोग उसकी बात बड़ी रुचि के साथ सुनते हैं। वहाँ पूर्ण शान्ति होती है। व्याख्याताओं को सुनने वालों की रुचि का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें बात करने में बल तथा उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि श्रोता गण दत्त-चित्त हैं अथवा नहीं। उन्हें विषय को थोड़ा बदलना चाहिए और कुछ नयी कहानियाँ सुनानी चाहिए और अनुकूल उदाहरण लाना चाहिए। उन्हें श्रोताओं की आँखों में सीधे देखना चाहिए। यदि कोई सफल व्याख्याता बनना चाहता है और श्रोताओं को एकाग्र बनाना चाहता है, तो उसे कई बातें जाननी आवश्यक हैं।
नेपोलियन, ग्लेडस्टोन, अर्जुन तथा ज्ञानदेव - सभी में अद्भुत एकाग्रता की शक्ति थी। वे अपने मन को किसी भी विषय पर एकाग्र कर सकते थे। सभी वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों में भी प्रशंसनीय स्तर का अवधान होता है। उन्होंने धैर्यपूर्वक नियमित और क्रमबद्ध अभ्यास द्वारा इसे अर्जित किया है। एक न्यायाधीश एवं सर्जन को उनके व्यवसाय में मात्र तभी अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी, जब कि उनमें अवधान की शक्ति उच्च स्तर की हो।
यदि आप कोई भी कार्य करें, तो उसमें लीन हो जायें। स्वयं को भूल आत्मा को डुबा दें। मात्र कार्य में ही ध्यान दें। सभी अन्य विचारों को रोक दें। जब आप एक कार्य करें, तो अन्य किसी कार्य के बारे में विचार न करें। जब आप एक पुस्तक पढ़ रहे हों, तो अन्य किसी पुस्तक के बारे में विचार न करें। अपने मन को उस तीर बनाने वाले की भाँति वहाँ लगायें, जिसे अपने चारों ओर की किसी बात का ध्यान ही नहीं था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में तथा शोधों में इतने व्यस्त और एकाग्र रहते हैं कि उन्हें दो दिन तक भोजन लेने का भी ध्यान नहीं रहता है। एक बार की बात है। एक वैज्ञानिक अपने कार्य में बहुत व्यस्त था। उसकी पत्नी जो कि किसी अन्य शहर में रहती थी, उसके ऊपर कोई संकट आ गया। वह दौड़ती हुई प्रयोगशाला में आयी, उसकी आँखों में आँसू थे। बड़े आश्चर्य की बात हुई! वह वैज्ञानिक थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। वह अपने कार्य में इतना तल्लीन था कि वह यह भी भूल गया कि वह उसकी अपनी पत्नी है। उसने कहा मैडम आप थोड़ी देर तक और रोयें। मुझे आपके आँसुओं का विश्लेषण कर लेने दें।
एक बार एक सम्भ्रान्त व्यक्ति ने श्री इशाक न्यूटन को रात्रि भोजन के लिए बुलाया। न्यूटन तैयार हो कर अपने मेजबान के घर गये और उसके हॉल में बैठ गये। वह व्यक्ति न्यूटन के बारे में सब कुछ भूल गया, उसने अपना रात्रि का भोजन किया और सो गया। न्यूटन तो विज्ञान के किसी प्रयोग के बारे में विचार के बारे में सोचते हुए इतना तल्लीन थे कि उन्हें इस रात्रि-भोजन के बारे में ध्यान ही न रहा। वे अपनी कुर्सी पर एक मूर्तिवत् बैठे रहे। अगली सुबह मेजबान ने न्यूटन को अपने मेहमानखाने में देखा, तो उसे ध्यान आया कि उसने न्यूटन को रात्रि भोजन पर आमन्त्रित किया था। उसे अपने भुलक्कड़पने पर दुःख हुआ और उसने न्यूटन से अत्यन्त दुःखी स्वर में क्षमा माँगी। न्यूटन की एकाग्रता की शक्ति कितनी अद्भुत थी! सभी मेधावी लोगों में यह शक्ति अनन्त स्तर तक होती है।
प्रोफेसर जेम्स के अनुसार हम चीजों की ओर इसलिए ध्यान देते हैं, क्योंकि वे बड़ी रुचिकर होती हैं। लेकिन प्रोफेसर पिल्सबेरी की यह धारणा है कि चीजें इसलिए रुचिकर लगती हैं, क्योंकि हम उन पर इसलिए ध्यान देते हैं, क्योंकि हम उन पर ध्यान देना पसन्द करते हैं। जब वे रुचिकर नहीं होतीं, तो हम उन पर ध्यान नहीं देते।
निरन्तर अभ्यास तथा एकाग्रता के नये-नये प्रयत्नों के द्वारा जब आप उसके स्वामी बन जाते हैं तथा उसके अर्थ और उसके परिणामों के बारे में जानने लगते हैं, तो कोई भी विषय जो कि प्रारम्भ में शुष्क तथा अरुचिकर लगता है, वही बाद में रुचिपूर्ण लगने लगता है। उस विषय पर आपके अवधान की धारणा शक्ति दृढ़ हो जायेगी।
जब आपके ऊपर कोई भी दुर्भाग्य आ पड़ता है अथवा आपको असफलता के कारणों की खोज हेतु पुरानी किसी बात का स्मरण करना होता है, तो आपके मन पर इसका इतना अधिक प्रभाव रहता है कि आप किसी भी तरह से इसके बारे में विचार करने से रुक नहीं पाते। एक लेख लिखना है अथवा एक पुस्तक पूरी होने वाली है, तो काम चालू रहता है, चाहे आपकी नींद का नुकसान हो, फिर भी आप स्वयं को इससे अलग करने में असमर्थ रहते हैं। अवधान स्वैच्छिक रूप से चेतना के सम्पूर्ण क्षेत्र पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है।
यदि आपके पास धारणा की अच्छी शक्ति हो, तो कोई भी बात जो मन ग्रहण करता है, वह गहरा प्रभाव डालती है। एक अवधान सम्पन्न व्यक्ति ही मात्र अपनी संकल्प शक्ति का विकास कर सकता है। अवधान, प्रयास तथा रुचि का मिश्रण आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। एक साधारण बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति जिसका अवधान अत्यधिक विकसित हो, वह उन उच्च बुद्धि सम्पन्न व्यक्तियों की तुलना में अधिक कार्य कर सकता है, जिनकी एकाग्रता की शक्ति कम विकसित है। किसी भी कार्य में असफलता का मूल कारण है अवधान की कमी। यदि एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दिया जाये, तो आपको उस विषय का तथा उसके विभिन्न रूपों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। संसार के सामान्य अप्रशिक्षित व्यक्ति सामान्यतया एक समय में कई बातों को ग्रहण करते हैं। वे अपनी मानसिक कार्यशाला के द्वार के भीतर कई चीजों को प्रवेश करने देते हैं और यही कारण है कि उनका मन धुंधला अथवा मलिन होता है। उनमें विचारों की स्पष्टता नहीं होती है। वे विश्लेषण और संश्लेषण नहीं कर सकते। वे भ्रमित रहते हैं। वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जब कि एक संयमित व्यक्ति किसी भी विषय पर जितनी देर तक चाहे ध्यान दे सकता है। वह किसी भी एक विषय अथवा वस्तु के बारे में पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है, तत्पश्चात् वह किसी अन्य विषय को कर सकता है। अवधान किसी भी योगी की महत्त्वपूर्ण योग्यता है।
आप एक ही समय में दो विभिन्न विषयों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। मन एक समय में दो विषयों पर ध्यान नहीं दे सकता है। चूँकि यह इतनी अद्भुत गति से आगे-पीछे जाता है कि आपको लगता है कि मन एक ही समय में कई विषयों पर ध्यान दे सकता है। आप एक समय में मात्र देख अथवा सुन सकते हैं। आप एक ही समय में देख और सुन नहीं सकते। लेकिन यह नियम विकसित योगी के ऊपर लागू नहीं होता। एक उच्च योगी एक ही समय में कई कार्य कर सकता है; क्योंकि उसका संकल्प दैवी संकल्प जो कि सर्वशक्तिमान् है, उससे पृथक् नहीं रहता।
२. धारणा का अभ्यास
मन को शरीर के भीतर अथवा बाहर किसी विषय पर केन्द्रित करें। कुछ देर वहीं स्थिर रहें। यह धारणा है। आपको इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए।
सबसे पहले उत्तम चरित्र के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कीजिए, तत्पश्चात् धारणा का अभ्यास प्रारम्भ कीजिए। मन की शुद्धता के बिना धारणा के अभ्यास से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुछ ऐसे तान्त्रिक हैं, जिनकी धारणा तो अच्छी होती है, किन्तु उनका चरित्र अच्छा नहीं होता। यही कारण है कि उनका आध्यात्मिक जीवन में किंचित् भी विकास नहीं होता।
जिसका आसन स्थिर है तथा जिसने श्वास पर नियन्त्रण द्वारा अपनी नाड़ियों तथा कोशों को शुद्ध कर लिया है, वह सरलता से धारणा कर लेता है। यदि आप सभी विचलनों को हटा दें, तो आपकी धारणा प्रबल होगी। एक सच्चा ब्रह्मचारी जिसने वीर्य का संरक्षण किया है, उसकी धारणा अद्भुत होती है।
कुछ अधैर्यवान् साधक बिना किसी नैतिक प्रशिक्षण के सीधे धारणा का अभ्यास करने लगते हैं। यह भयंकर भूल है। नैतिक पूर्णता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।
आप आध्यात्मिक ऊर्जा के सातों केन्द्रों में से किसी एक पर धारणा कर सकते हैं। अवधान धारणा में बड़ी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसने अवधान की शक्ति का विकास कर लिया है, उसकी धारणा अच्छी होती है। वह व्यक्ति जो वासनाओं एवं काल्पनिक कामनाओं से पूर्ण है, वह किसी भी विषय अथवा वस्तु पर मुश्किल से एक सेकेंड तक ही धारणा कर सकता है। उसका मन एक बूढ़े बन्दर की भाँति कूदता रहता है।
वह जिसने प्रत्याहार (इन्द्रियों को विषयों से वापस खींचना) प्राप्त कर लिया है, उसकी धारणा अच्छी होती है। आपको आध्यात्मिक पथ में एक-एक कदम, एक-एक अवस्था करके आगे बढ़ना होगा। अभ्यास प्रारम्भ करने के लिए उत्तम चरित्र, आसनों, प्राणायाम और प्रत्याहार की नींव डालें। तभी धारणा और ध्यान का भव्य भवन सफलतापूर्वक खड़ा होगा।
आपको धारणा के विषय को उसकी अनुपस्थिति में भी देखने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मानसिक चित्र एक क्षण में ही आपके सामने आ जाना चाहिए। यदि आपकी धारणा होगी, तो आप यह कार्य बिना किसी कठिनाई के कर सकेंगे। अभ्यास के प्रारम्भ में आप घड़ी की टिक-टिक या मोमबत्ती की लौ अथवा अन्य किसी भी सुखकर विषय पर जो मन को अच्छा लगे, धारणा कर सकते हैं। यह स्थूल धारणा है।
मन को विश्राम लेने के स्थान के बिना धारणा सम्भव ही नहीं। प्रारम्भ में मन किसी भी उस विषय पर एकाग्र किया जा सकता है, जो सुखकर हो। इसे प्रारम्भ में किसी भी ऐसे विषय पर एकाग्र करना सम्भव नहीं, जिसे मन पसन्द न करता हो। पद्मासन में बैठ जायें। दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर टिकायें। इसे नासिकाग्र दृष्टि कहते हैं। किसी प्रकार का हिंसात्मक प्रयास न करें। नासिका के अग्र भाग पर सहजता से देखते रहें। प्रारम्भ में मात्र एक मिनट तक अभ्यास करें। धीरे-धीरे इस समय को आधा घण्टे अथवा इससे अधिक बढ़ायें। यह अभ्यास मन को स्थिर करता है। यह धारणा-शक्ति का विकास करता है। जब आप पैदल चलते हैं, तो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। पद्मासन में बैठ जायें और मन को दोनों भौहों के बीच में एकाग्र करने का प्रयत्न करें। इसे आधा मिनट तक सहज रूप से करें। फिर इसका समय शनैः-शनैः आधा घण्टे अथवा और अधिक बढ़ायें। अभ्यास में तनिक भी हिंसात्मकता नहीं होनी चाहिए। यह अभ्यास मन का विचलन दूर करता है और धारणा का विकास करता है। इसे भ्रूमध्य-दृष्टि कहते हैं। आप अपनी रुचि, स्वभाव एवं क्षमता के अनुसार नासिकाग्र-दृष्टि अथवा भ्रूमध्य-दृष्टि का चुनाव कर सैकते हैं।
यदि आप अपनी धारणा-शक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसारिक गतिविधियाँ कम करनी होंगी। आपको प्रतिदिन दो घण्टे अथवा अधिक देर तक मौन का पालन करना होगा।
तब तक धारणा का अभ्यास करें, जब तक मन धारणा के विषय पर स्थिर न हो जाये। जब मन धारणा के विषय से भागे, इसे पुनः वापस ले आयें।
जब धारणा गहन और प्रबल होगी, अन्य इन्द्रियाँ कार्य नहीं कर सकेंगी। जो नित्य तीन घण्टे तक धारणा का अभ्यास करता है, उसके पास अद्भुत सिद्धियाँ होती हैं। उसके पास दृढ़ संकल्प-शक्ति होती है।
३. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धारणा
धारणा आध्यात्मिक पथ के प्रारम्भिक अभ्यासियों के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग्यता है। धारणा आध्यात्मिक पथ में ही नहीं, वरन् जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। धारणा के बिना मनुष्य जीवन में असफल रहता है।
आध्यात्मिक अर्थ में धारणा का अर्थ है-चित्त की एकाग्रता अर्थात् किसी इष्टदेवता अथवा देवी के ऊपर मन को स्थिर करना। धारणा की प्राप्ति के लिए आपको संसार के सभी निरर्थक विचारों को दूर हटाना होगा। आपको सांसारिक प्रवृत्ति की सभी आधारभूत कामनाओं से पूर्णतः मुक्त होना होगा। आपको उनके स्थान पर दैवी विचारों को प्रतिस्थापित करना होगा।
धारणा के बाद ध्यान आता है। ध्यान के बाद समाधि आती है। निर्विकल्प समाधि जो सभी प्रकार के द्वैत विचारों से मुक्त होती है, उसके पश्चात् जीवन्मुक्त स्थिति आती है। जीवन्मुक्त स्थिति जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर प्रेरित करती है। इसलिए जो साधक आध्यात्मिक पथ का अवलम्बन करना चाहते हों, उनके लिए धारणा सर्वप्रथम आवश्यकता है।
प्रत्येक छोटे से कार्य हेतु धारणा एवं सम्पूर्ण हृदय से एकाग्रता की माँग होती है। यदि आप किसी सुई के छेद में धागा डालना चाहते हैं, तो आपको धागे से निकले हुए सभी छोटे-छोटे तन्तुओं को हटा कर इसे एक तन्तु बनाना पड़ेगा और बड़ी ही सावधानीपूर्वक स्थिर चित्त विचार से धागे को छेद में डालना होगा।
जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं अथवा ढाल पर उतरना चाहते हैं, तो आपको बड़ा ही सावधान रहना चाहिए अन्यथा आप फिसल जायेंगे और गहरी खाई में गिर जायेंगे। यदि आप साइकिल पर सवारी करते समय अपने मित्र से बातें कर रहे हैं, तो कोई कार आपको पीछे से धक्का मार सकती है। यदि आपका ध्यान सड़क पर चलते समय नहीं होगा, तो आप किसी पत्थर से टकरा जायेंगे और गिर पड़ेंगे। एक असावधान नाई अपने ग्राहक की नाक काट देगा। एक असावधान धोबी अपने मालिक के कपड़े जला देगा। ध्यान के न होने पर एक सुस्त जिज्ञासु अपना सिर दीवार में मार देगा और भूमि पर चारों खाने चित्त गिर पड़ेगा। इसलिए आपको अवधान का विकास करना चाहिए। अवधान धारणा की ओर ले जाता है।
अपने मन को हाथ में लिये गये कार्य पर लगायें। अपना सम्पूर्ण हृदय और आत्मा कार्य पर लगायें। चाहे यह केले का छिलका छीलने अथवा नीबू निचोड़ने जैसा साधारण कार्य ही क्यों न हो। किसी भी कार्य को बेतरतीब ढंग से न करें। कभी भी जल्दबाजी में भोजन न करें। अपने सभी कामों में शान्त और धैर्यवान् रहें। कभी भी किसी कार्य में जल्दबाजी न करें। शान्ति तथा एकाग्रता के बिना कोई भी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं होता। जिन्होंने सफलता प्राप्त की और महान् बने, उन सभी में यह गुण अनिवार्य रूप से उपस्थित था।
यदि आप अपने सभी कार्य पूर्ण अवधान और एकाग्रता के साथ करेंगे, तो आप अपने प्रत्येक प्रयास में सफल होंगे। जब आप प्रार्थना एवं ध्यान हेतु बैठें, तो कभी भी अपने ऑफिस के काम के बारे में न सोचें। जब आप ऑफिस में काम कर रहे हों, तो अपने बच्चे के बारे में जो घर पर बीमार है अथवा घर के किसी अन्य कार्यों के बारे में विचार न करें। जब आप स्नान करें, तो खेल के बारे में विचार न करें। जब आप भोजन करें, तो ऑफिस में जो कार्य शेष है, उसके बारे में विचार न करें। आपको स्वयं को हाथ में लिये गये कार्य को पूर्ण एकाग्रता से करने का प्रशिक्षण देना होगा। आप सरलतापूर्वक अपनी स्मरण शक्ति तथा संकल्प शक्ति का विकास कर सकते हैं। धारणा विजय के द्वार को खोलने की चाबी है। यदि एक साधारण व्यक्ति किसी काम को करने में एक घण्टा लगाता है, तो अच्छी धारणा वाला व्यक्ति उसी काम को पहले वाले की तुलना में अधिक कुशलता से और आधे घण्टे में ही पूरा कर लेगा। आप इसके (धारणा के अभ्यास) द्वारा महान् बन जायेंगे ।
आपको मन के शिथिलीकरण की विद्या का ज्ञान होना चाहिए। आपको मन से अन्य विचारों को बाहर निकालने की विधि का ज्ञान होना चाहिए। आपको इस समय मात्र विश्राम के बारे में ही सोचना चाहिए। आपको स्वयं को मृत समझना चाहिए। ईश्वर के नाम का जप कीजिए और उनके गुणों के आनन्द स्वरूप का विचार कीजिए। आपको निद्रा के समय स्वप्न नहीं आना चाहिए। तब आपको अच्छी नींद आयेगी और आप अत्यन्त सरलता से ताजा हो जायेंगे। यदि आप दो घण्टे भी सो लेंगे, तो भी आप ताजा अनुभव करेंगे।
४. धारणा के योग का आश्रय स्थल
यह कहना बड़ा ही कठिन है कि कहाँ से धारणा समाप्त होती है और कहाँ से ध्यान प्रारम्भ होता है। ध्यान धारणा का अनुकरण करता है। सर्वप्रथम यम-नियम के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कीजिए। तत्पश्चात् धारणा का अभ्यास प्रारम्भ कीजिए। बिना शुद्धता के धारणा निरर्थक है।
मन की स्थिरता धारणा है। यदि आप विचलनों के सभी कारणों का उन्मूलन कर दें, तो आपकी धारणा-शक्ति में वृद्धि हो जायेगी। एक सच्चा ब्रह्मचारी जिसने अपने वीर्य का संरक्षण किया है, उसकी धारणा शक्तिशाली होगी। धारणा में अवधान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसने अवधान की शक्ति का विकास कर लिया है, उसकी धारणा अच्छी होती है। आपको धारणा के विषय को उसकी अनुपस्थिति में भी स्पष्ट रूप से देख सकना चाहिए। एक ही क्षण में उसका मानसिक चित्र आपके सामने आ जाना चाहिए। यदि आपको धारणा का अच्छा अभ्यास हो, तो आप इसे बिना किसी कठिनाई के कर सकेंगे। वह जिसने विभिन्न विषयों से इन्द्रियों को वापस खींच कर प्रत्याहार में सफलता प्राप्त कर ली है, उसकी धारणा अच्छी होती आपको आध्यात्मिक पथ में चरण दर चरण एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक बढ़ना होगा। अभ्यास प्रारम्भ करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की नींव डालें। धारणा, ध्यान, समाधि का भव्य भवन तभी सफलतापूर्वक खड़ा होगा।
आसन बहिरंग साधना है। ध्यान अन्तरंग साधना है। जब ध्यान और समाधि के साथ तुलना की जाये, तो धारणा भी बहिरंग साधना है। वह जिसका आसन स्थिर है, जिसने प्राणायाम द्वारा योग-नाड़ियों तथा प्राणमय कोश का शुद्धिकरण कर लिया हो, वह सरलतापूर्वक धारणा कर सकता है। आप आन्तरिक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा के सातों चक्रों (मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र तथा सहस्रार) में से कोई एक, नासिकाग्र, जिह्वा की नोंक अथवा बाह्य रूप से किसी देवता जैसे हरि, हर, कृष्ण अथवा देवी के चित्र पर धारणा कर सकते हैं। आप घड़ी की टिक-टिक ध्वनि, मोमबत्ती की लौ, दीवाल पर कोई काला बिन्दु, पेंसिल, गुलाब का फूल अथवा किसी सुखकर विषय पर भी धारणा कर सकते हैं। यह स्थूल धारणा है। मन के विश्राम हेतु किसी वस्तु के बिना धारणा सम्भव ही नहीं है। मन को किसी भी सुखकर विषय जैसे चमेली का फूल, आम, सन्तरा अथवा प्रिय मित्र पर सरलता से स्थिर किया जा सकता है। प्रारम्भ में मन को किसी ऐसे विषय पर एकाग्र करना कठिन है जिसे यह नापसन्द करता हो जैसे मल, कोबरा, शत्रु, कुरूप चेहरा आदि। धारणा का अभ्यास तब तक करें, जब तक कि मन धारणा के विषय पर अच्छी तरह स्थापित हो जाये। जब मन धारणा के विषय से दूर भागे, तो इसे पुनः धारणा के विषय पर वापस खींच कर ले आये। गीता में भगवान् कृष्ण कहते हैं— “यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥” जब-जब घुमन्तु तथा अस्थिर मन भागे, तब-तब इसे वश में करके आत्मा के नियन्त्रण में ले कर आयें।
यदि आप अपनी धारणा-शक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसारिक गतिविधियाँ कम करनी होंगी (व्यवहार-क्षय)। आपको नित्य दो घण्टे का मौन भी रखना होगा। एक व्यक्ति जिसका मन वासनाओं तथा काल्पनिक इच्छाओं से परिपूर्ण है, वह मन को किसी भी विषय पर कठिनाई से एक क्षण के लिए ही एकाग्र कर सकेगा। उसका मन एक गुब्बारे की भाँति कूदता रहता है। अपनी श्वास का नियमन तथा नियन्त्रण करें। इन्द्रियों को वश में करें और मन को किसी सुखकर विषय पर केन्द्रित करें। धारणा के विषय के साथ पवित्रता तथा शुद्धता के विचारों को संयुक्त करें।
आप भ्रूमध्य (अथवा त्रिकुटी) पर धारणा कर सकते हैं। आप अपने दाहिने कान से सुनायी पड़ने वाली अनाहत ध्वनियों पर धारणा कर सकते हैं। आप ॐ के चित्र पर धारणा कर सकते हैं। मुरली हाथ में लिये भगवान् कृष्ण, तथा शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथों में लिये हुए भगवान् विष्णु का चित्र धारणा हेतु बहुत अच्छे हैं। आप अपने गुरु अथवा किसी सन्त के चित्र पर धारणा कर सकते हैं। वेदान्ती मन को आत्मा पर एकाग्र करते हैं। यह उनकी धारणा है।
धारणा अष्टांगयोग अथवा पतंजलि महर्षि के राजयोग की छठवीं अवस्था या अंग है। धारणा में आपके मन की झील में मात्र एक ही वृत्ति या लहर होगी तथा मन मात्र एक ही विषय का रूप ग्रहण करेगा। मन के सभी अन्य कार्य रुक जायेंगे। जो व्यक्ति आधे घण्टे या एक घण्टे के लिए भी सच्चा ध्यान करता है, उसके पास अद्भुत सिद्धियाँ होती हैं। उसकी संकल्प-शक्ति बड़ी ही प्रबल होती है।
जब हठयोगी अपने मन को षट चक्रों पर एकाग्र करते हैं, तो वे अपने मन को उनसे सम्बन्धित अधिष्ठाता देवता जैसे गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव पर भी एकाग्र करते हैं। प्राणायाम द्वारा श्वास को नियन्त्रित करके, इन्द्रियों को प्रत्याहार द्वारा वश में करें, तत्पश्चात् मन को सगुण अथवा निर्गुण ब्रह्म पर केन्द्रित करें। हठयोग के अनुसार वह योगी जो कुम्भक के द्वारा अपनी श्वास को बीस मिनट तक रोक सकता है, उसकी धारणा बहुत अच्छी होती है। प्राणायाम मन को स्थिर करता है, मन के विक्षेप दूर करता है और धारणा-शक्ति में वृद्धि करता है। जो जिह्वा की निचली झिल्ली को काटने के द्वारा इसे लम्बी करके, इसे जिह्वा के ऊपर स्थित छिद्र में प्रविष्ट करा के ऊपर ले जा कर खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है, उसकी धारणा अच्छी होती है।
जो धारणा का अभ्यास करते हैं, वे शीघ्र विकास करते हैं। वे किसी भी कार्य को वैज्ञानिक रूप से सटीक ढंग से तथा अत्यन्त दक्षतापूर्वक कर सकते हैं। जो कार्य अन्य लोग छह घण्टे में करते हैं, वही कार्य धारणा सम्पन्न व्यक्ति आधे घण्टे में कर सकता है।
जिसे अन्य छह घण्टे में पढ़ते हैं, उसे ही अच्छी धारणा से सम्पन्न व्यक्ति आधे घण्टे में पढ़ सकता है। धारणा उमड़ते विचारों को शान्त करती है, शुद्ध करती है, विचार-शक्ति को बल प्रदान करती है तथा विचारों को स्पष्ट करती है। धारणा भौतिक समृद्धि में भी सहायता करती है। धारणा सम्पन्न व्यक्ति अपने कार्यालय अथवा व्यवसाय-गृह में भी अच्छा कार्य करता है। इसके पूर्व जो भी धुंधला तथा अस्पष्ट था, वह अब स्पष्ट और निश्चित हो जाता है। जो पहले कठिन था, वह अब सरल हो जाता है और जो पहले जटिल, भ्रमित करने वाला था, वह अब सरलता से समझ में आने लगता है। आप धारणा के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो नित्य धारणा का अभ्यास करता है, उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। जब कोई भूखा हो अथवा किसी जटिल रोग से पीड़ित हो, तो उसके लिए धारणा का अभ्यास करना बहुत कठिन है। जो धारणा का अभ्यास करता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी मानसिक दृष्टि अत्यन्त स्पष्ट होती है।
एक शान्त कमरे में पद्मासन में बैठ जायें। अपनी आँखें बन्द कर लें। जब आप एक सेब फल पर धारणा करते हैं, तो क्या होता है, देखें। आप इसके रंग, आकार, इसके विभिन्न भागों जैसे छिलके, गूदा, बीज आदि के बारे में विचार करते हैं। आप उन स्थानों के बारे में विचार कर सकते हैं, जहाँ से यह आया होता है। आप इसके अम्लीय अथवा मधुर स्वाद के बारे में तथा पाचन-तन्त्र और रक्त पर इसके प्रभावों के बारे में विचार कर सकते हैं। संयोजन के सिद्धान्त के अनुसार, किसी अन्य फल के विचार भी प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। मन कुछ अन्य बाह्य विचारों का भी आनन्द लेना चाहेगा। यह आश्चर्य भी कर सकता है। यह किसी मित्र से शाम ४ बजे रेलवे स्टेशन पर मिलने के बारे में विचार कर सकता है। यह एक तौलिया अथवा चाय के डिब्बे अथवा बिस्किट खरीदने के बारे में विचार कर सकता है। यह किसी अनहोनी के बारे में विचार कर सकता है, जो कि पिछले दिनों घटी हो। आपको विचारों की एक निश्चित रेखा पर विचार करने का प्रयास करना है। विचार की रेखा के बीच कोई अन्तराल नहीं होना चाहिए। आपको उन विचारों को भीतर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, जो विषय से सम्बन्धित नहीं । आपको इस दिशा में सफलता प्राप्ति हेतु कड़ा संघर्ष करना होगा। मन पुरानी लीकों की ओर भागने तथा अपने पुराने जाने-पहचाने रास्ते पर जाने का पूरा प्रयत्न करेगा। आपका यह प्रयास चढ़ाई चढ़ने जैसा होगा। जब आपको धारणा में कुछ सफलता मिलेगी, तो आपको आनन्द का अनुभव होगा। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम तथा संयोजन का नियम आदि भूमण्डल पर कार्य करते हैं, उसी प्रकार विचारों के निश्चित नियम जैसे निरन्तरता का नियम आदि मानसिक धरातल अथवा विचार-जगत् में कार्य करते हैं।
जो धारणा का अभ्यास करते हैं, उन्हें इन नियमों को अच्छी तरह समझना चाहिए। जब मन किसी विषय के बारे में सोचता है, तो यह इसके भागों के बारे में, इसके गुणों के बारे में भी विचार करता है। जब यह इसके कारण के बारे में विचार करता है, तो इसके प्रभाव के बारे में भी विचार करता है।
यदि आप भगवद्गीता, रामायण अथवा भागवत के ११ वें स्कन्ध को एकाग्रता के साथ कई बार पढ़ें, तो आपको प्रत्येक बार नये विचार प्राप्त होंगे। धारणा के द्वारा आपको सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि प्राप्त होगी, मानसिक चेतना के धरातल पर सूक्ष्म गुप्त अर्थ प्रकट होंगे। आप दार्शनिक महत्त्व की आन्तरिक गहराइयों को समझ सकेंगे। जब आप किसी विषय पर धारणा करें, तो मन से संघर्ष न करें। शरीर अथवा मन में यदि कहीं भी तनाव हो, तो उसे हटा दें। विषय के बारे में निरन्तर सहजता से विचार करें। मन को इधर-उधर न भागने दें।
यदि आवेग आपको धारणा के समय बाधा डालें, तो उन पर ध्यान न दें। वे शीघ्र चले जायेंगे। यदि आप उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, तो आप अपनी संकल्प शक्ति को आहत करेंगे। निरपेक्ष व्यवहार रखें। वेदान्ती इस सूत्र का प्रयोग करते हैं- मैं परवाह नहीं करता। बाहर जाओ। मैं साक्षी हूँ (सभी मानसिक रूपान्तरों का साक्षी)।" आवेगों को दूर भगाने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं और भगवान् के पास से सहायता आती है।
धारणा में मन को विभिन्न विषयों स्थूल और सूक्ष्म तथा विभिन्न आकारों मध्यम और बड़े हेतु प्रशिक्षित कीजिए। थोड़े समय में धारणा की दृढ़ आदत बन जायेगी। जिस क्षण आप ध्यान हेतु बैठेंगे, उसी क्षण मन सरलता से तैयार हो जायेगा। जब आप किसी पुस्तक का अध्ययन करें, तो उसे पूर्ण एकाग्रता से पढ़ें। जल्दी-जल्दी पृष्ठ उलटने का कोई लाभ नहीं है। गीता का एक पृष्ठ पढ़ें, उसके बाद पुस्तक को बन्द कर दें। जो आपने पढ़ा है, उस पर धारणा करें। महाभारत, उपनिषद् तथा भागवत में उसके समानान्तर वाक्य ढूँढ़ें। इनकी तुलना करें और इनमें अन्तर करें।
एक नवाभ्यासी के लिए धारणा का अभ्यास प्रारम्भ में अरुचिकर और थका देने वाला होता है। उसे मन और मस्तिष्क में नयी लीकें काटनी पड़ती हैं। कुछ माह पश्चात् उसे धारणा में रुचि हो जाती है। उसे एक नये प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है। वह आनन्द है— धारणा का आनन्द। यदि वह एक दिन के लिए भी इस नये प्रकार के आनन्द को नहीं प्राप्त कर पाता, तो उसे बेचैनी का अनुभव होता है।
संसार के दुःखों एवं कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय धारणा है। आपका एकमात्र कर्तव्य है धारणा का अभ्यास करना। आपने इस शरीर को धारणा के अभ्यास तथा इस अभ्यास के द्वारा आत्मा के साक्षात्कार हेतु धारण किया है। दान, राजसूय यज्ञ आदि की यदि धारणा के साथ तुलना की जाये, तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। ये खिलौने मात्र हैं।
वैराग्य, प्रत्याहार और धारणा के अभ्यास से चंचल मन की बिखरी हुई किरणें धीरे-धीरे एकत्रित हो जाती हैं। स्थिर अभ्यास से यह एकाग्रचित्त हो जाता है। वह योगी कितना प्रसन्न और दृढ़ है, जिसका चित्त एकाग्र है। वह पलक झपकने के भीतर ही ढेर सारा काम कर सकता है।
जो धारणा का अभ्यास कभी करते हैं और कभी बन्द कर देते हैं, उनका मन कभी-कभी ही स्थिर होता है। कभी-कभी मन भ्रमण करने लगता है और उस समय यह प्रयोग हेतु एकदम निरुपयोगी होता है। आपका मन ऐसा होना चाहिए कि वह सदैव गम्भीरतापूर्वक आपके आदेशों का पालन करे और किसी भी समय आपके दिये गये आदेशों को यथासम्भव अच्छी तरह पूरा करके लाये। राजयोग का स्थिर और क्रमबद्ध अभ्यास मन को अत्यन्त आज्ञापालक तथा विश्वसनीय बनाता है।
मन की पाँच स्थितियाँ अथवा योग-भूमिकाएँ हैं जैसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। धारणा के धीरे-धीरे एवं पूर्ण नियमित अभ्यास से चंचल मन की बिखरी हुई किरणें एकत्रित हो जाती हैं। यह एकाग्र हो जाता है और स्वाभाविक रूप से यह वश में आ जाता है। यह उचित नियन्त्रण में आ जाता है।
यदि साधक जो उपयुक्त नहीं है उसका अनुकरण करता है, तो उसकी प्रगति कठिनाई से तथा अवरुद्ध होती है। जो सही पथ का चुनाव करता है, उसकी प्रगति सरलता से होती है एवं उसे शीघ्र अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है। जिसके पूर्व-जन्म के आध्यात्मिक संस्कार नहीं है, उसकी प्रगति कष्टप्रद होती है। जिसके आध्यात्मिक संस्कार हैं, उसकी प्रगति सरलता से होती है। जिसका स्वभाव दुष्ट है और जिसकी नियन्त्रण- क्षमता दुर्बल है, उसकी प्रगति कष्टप्रद एवं बाधित होगी; लेकिन जिसकी संयम की क्षमता अच्छी है, उसकी प्रगति शीघ्र होगी तथा उसे शीघ्र अन्तर्दृष्टि प्राप्त होगी। जो अज्ञानता से घिरा हुआ है, उसकी अन्तर्दृष्टि बाधित होगी और जो ऐसा नहीं होगा, उसे अन्तर्दृष्टि शीघ्र प्राप्त होगी।
५. धारणा हेतु अभ्यास
● १. अपने मित्र से कुछ ताश के पत्ते दिखाने के लिए कहें। देखने के तुरन्त पश्चात् आपने जो भी पत्ते देखे हैं, उनके बारे में, उनके नाम तथा संख्या, जैसे हुक्म का बादशाह, ईंट का दहला, चिड़ी की बेगम, पान का जोकर आदि बतायें।
● २. किसी पुस्तक के दो-तीन पृष्ठ पढ़िए, इसके बाद पुस्तक को बन्द कर दें। अब जो आपने पढ़ा है, उस पर विचार करें। सभी अन्य विचारों की उपेक्षा कर दें। सावधानीपूर्वक अपने ध्यान को केन्द्रित करें। मन को संयोजन, वर्गीकरण, समूहीकरण एवं तुलना करने दें। आपको अब विषय का बहुत-सा ज्ञान और सूचना प्राप्त होगी। असावधानीपूर्वक पन्ने उलटने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे कई विद्यार्थी हैं, जो किसी पुस्तक को कुछ घण्टों में ही पढ़ लेते हैं; लेकिन जब आप उनसे पुस्तक के कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में जानना चाहेंगे, तो वे निरुत्तर हो जायेंगे। यदि आप हाथ में लिये गये विषय को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, तो आपको स्पष्ट और दृढ़ अनुभव प्राप्त होंगे। यदि ये अनुभव गहरे और दृढ़ होंगे, तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी ।
● ३. घड़ी से एक फुट दूर अपने प्रिय ध्यान के आसन में बैठ जाइए। घड़ी की टिक-टिक की ध्वनि पर धारणा करें। जब-जब मन भागे, बार-बार इस ध्वनि सुनने का प्रयास करें। जरा देखिए, मन कितनी देर तक ध्वनि पर निरन्तर दृढ़ रहता है।
● ४. पुनः अपने प्रिय आसन में बैठ जायें। अपनी आँखें बन्द कर लें। अपने कानों को अँगूठों से अथवा मोम या रुई से बन्द कर लें। अनाहूत ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें। आपको विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ जैसे बाँसुरी, तूफान, शंख, घण्टियों की ध्वनि, मधुमक्खी के भिनभिनाने की ध्वनि आदि सुनायी देगी। सबसे पहले स्थूल ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। एक ही प्रकार की ध्वनि सुनने का प्रयास करें। यदि मन भागे, तो आप इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर अथवा सूक्ष्म से स्थूल की ओर स्थानान्तरित कर सकते हैं। सामान्यतया आप दाहिने कान से ध्वनि सुन सकेंगे। कभी-कभी आपको बायें कान से ध्वनि सुनायी देगी। लेकिन किसी एक कान की ध्वनि से चिपके रहने का प्रयास करें। आपको चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। यह मन को पकड़ने का सरल तरीका है; क्योंकि मन मधुर ध्वनि के द्वारा उसी प्रकार मोहित हो जाता है, जिस प्रकार सर्प सँपेरे की बीन पर मोहित हो जाता है।
● ५. अपने सामने जलती हुई मोमबत्ती रखें और इसकी लौ पर धारणा करने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करते हुए थक जायें, तो अपनी आँखें बन्द कर लें और ज्योति को देखने का प्रयास करें। ऐसा आधे मिनट तक करें और धीरे से इस समय को अपनी रुचि, स्वभाव तथा क्षमता के अनुसार पाँच से दस मिनट तक बढ़ायें। जब आप गहन ध्यान में होंगे, तो आपको ऋषियों तथा देवताओं के दर्शन होंगे।
● ६. लेट कर चन्द्रमा पर धारणा करें। जब भी मन भागे, तो इसे बार-बार चन्द्रमा की ओर ले कर आयें। यह धारणा भावुक प्रकृति वाले व्यक्तियों में बड़ी ही उपयोगी है।
● ७. उपर्युक्त प्रकार से आप अपने सिर पर चमक रहे अरबों सितारों में से किसी एक सितारे पर धारणा कर सकते हैं।
● ८. आप एक नदी के किनारे बैठ जायें, जहाँ इसकी 'ॐ' की भाँति ध्वनि सुनायी दे रही हो। इस ध्वनि पर जब तक आप चाहें, धारणा करें। यह अत्यन्त उत्साहजनक और प्रेरक होती है।
● ९. खुली हवा में लेट जायें और ऊपर नीले विस्तृत आकाश पर धारणा करें। आपका मन तत्क्षण उन्नत हो जायेगा। आपका आत्मोत्थान होगा। नीला आकाश आपको आत्मा की अनन्त प्रकृति का स्मरण करायेगा।
● १०. एक आरामदायक आसन में बैठ जायें और अनेक सद्गुणों जैसे करुणा, सहिष्णुता आदि में से किसी एक पर धारणा करें। जितनी देर तक सम्भव हो, इस गुण में लीन होने का प्रयास करें।
६. कुर्सी पर धारणा
नवाभ्यासी के लिए धारणा का विषय प्रारम्भ में बड़ा ही उबाऊ और थका देने वाला होता है। लेकिन यह संसार में सर्वाधिक रुचिकर और लाभदायक विद्या है। जब कोई धारणा में आगे बढ़ता है और उसका सच्चा विकास होता है, अथवा जब उसे कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, तो वह अभ्यास नहीं छोड़ सकता। तब वह धारणा के अभ्यास के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। यदि वह किसी दिन अभ्यास नहीं कर पाता है, तो वह बेचैन हो जाता है। धारणा परमानन्द, आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति, सच्चा सन्तोष तथा अनन्त आन्तरिक शान्ति प्रदान करती है। धारणा से प्रचुर ज्ञान, गहन अन्तर्दृष्टि, अन्तःप्रेरणा तथा ईश्वर से मिलन प्राप्त होता है। यह तीनों लोकों में अद्भुत विद्या है। मैं इसके लाभों का पूर्णतया वर्णन करने में असमर्थ हूँ।
कुर्सी पर धारणा का अर्थ है—कुर्सी के विभिन्न भागों के बारे में विचार करना, उस विशेष लकड़ी के बारे में विचार करना जिससे यह निर्मित है— जैसे देवदार, शीशम आदि, इसकी कार्य-क्षमता, इसकी मजबूती, इसका मूल्य तथा यह पीठ, हार्थो आदि को जो आराम प्रदान करती है, उसके स्तर आदि के बारे में विस्तृत विचार करना।
इसके भाग अलग किये जा सकते हैं अथवा नहीं, यह आधुनिक ढंग से निर्मित है तथा दीमक से सुरक्षित है या नहीं, इसे सुरक्षित बनाने के लिए कौन-सी पालिश या वार्निश का उपयोग किया गया है आदि के बारे में विचार ।जब आप कुर्सी पर धारणा करेंगे, तो आपके मन में इस प्रकार के विचार आयेंगे। मन सामान्य रूप से निरुद्देश्य रूप से जंगली पशु की भाँति भटकता रहता है। यह एक विषय के बारे में विचार करता है और एक ही सेकेंड के भीतर यह उसे छोड़ कर एक बन्दर की तरह दूसरे विषय की ओर चला जाता है, तत्पश्चात् तीसरे विषय की ओर चला जाता है और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। यह एक बिन्दु पर टिका ही नहीं रह सकता।
जब विचार एक निश्चित लीक में मात्र एक ही विषय पर ही तैलधारावत् चले, तो यह धारणा है। जिज्ञासु को जब-जब उसका मन बाहर भागे, तो उसे वापस खींचना चाहिए और उसे उसी लीक में एक ही विचार की रेखा में एक ही विषय और एक ही धारणा पर रखना चाहिए। यह आध्यात्मिक साधना है। यह धारणा और ध्यान है। यह समाधि अथवा परम चेतनावस्था, चतुर्थ स्थिति या तुरीयावस्था में परिणित हो जाती है।
धारणा में महत्त्वपूर्ण है प्रारम्भ में मन की गतिविधियों को एक छोटे चक्र में समेट कर उसे पुनः विषय के उसी बिन्दु पर लाना। यही मुख्य लक्ष्य है। एक समय आयेगा, जब यह एक बिन्दु पर टिका रहेगा। यह आपकी निरन्तर और दीर्घकालीन साधना का परिणाम होगा। यह अवस्था आने पर प्राप्त होने वाला आनन्द अवर्णनीय होगा जब आप एक कुर्सी पर धारणा करेंगे, तो मात्र कुर्सी से सम्बन्धित सभी विचारों को लायें और उन विचारों में डूब जायें। अन्य विचारों को मन के भीतर प्रवेश न करने दें। इस समय विचारों की एक ही रेखा होनी चाहिए। इसमें एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल के निरन्तर प्रवाह की भाँति (तैलधारावत् प्रवाह) अथवा चर्च के घण्टे की निरन्तर आती आवाज की तरह विचारों की एक निरन्तरता होनी चाहिए। इस समय एक विषय से सम्बन्धित अनेक विचार हो सकते हैं। आप एक विषय से सम्बन्धित विचारों की संख्या को कम कर सकते हैं और एक विषय से सम्बन्धित एक विचार पर आ सकते हैं। जब यह एक विचार भी मृत हो जायेगा, तो आप परम चेतना या समाधि अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। जब एक ही विचार होता है, तो इसे सविकल्प समाधि कहते हैं, जो कि निम्न अवस्था है। जब यह एक विचार भी मृत हो जाता है, जब वहाँ एक विचार भी नहीं रहता, तो मन रिक्त बन जाता है। तब वहाँ मानसिक भाव-शून्यता होती है। यह पतंजलि महर्षि के राजयोग दर्शन में निर्विचार अवस्था है। आपको इस रिक्त वृत्ति से भी ऊपर उठना है और स्वयं को परम पुरुष अथवा ब्रह्म जो कि मन का मौन साक्षी है तथा जो मन को शक्ति एवं प्रकाश प्रदान करता है, के साथ एक करना है। मात्र तभी आप जीवन के परम लक्ष्य तक पहुँचेंगे।
जब आप कुर्सी पर धारणा करें, तो विभिन्न विषयों के अन्य विचारों को प्रवेश न करने दें। घुमक्कड़ मन को बार-बार विषय पर जो कि कुर्सी है, वापस ले कर आयें। जब आप गुलाब का ध्यान करें, तो मात्र गुलाब के बारे में ही विचार करें। जब आप किसी पुस्तक के बारे में सोचें, तो वह सब सोचें जो कि पुस्तक से सम्बन्धित है, इससे बाहर का कुछ न सोचें। जब आप रेडियो अथवा टीवी के बारे में विचार करें, तो मात्र रेडियो और टीवी के बारे में ही विचार करें। हाथ में लिये गये विषय से सम्बन्धित सभी बातों को खाली कर दें। आप मन के प्रिय किसी भी विषय को ले सकते हैं। धीरे से आप रुचि उत्पन्न करके ऐसा विषय जो मन को अप्रिय हो, उसे भी ले सकते हैं। आपको सदा इस सूत्र को स्मरण रखना चाहिए- "एक समय में एक काम और अच्छी प्रकार से किया गया। यह बहुत अच्छा नियम है। ऐसा कई लोगों ने बताया है।" जब आप कोई भी काम हाथ में लें, अपना सम्पूर्ण हृदय, पूर्ण मन और आत्मा इसमें लगायें। इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ करें। जो अन्य छह घण्टों में कर सकते होंगे, वह आप आधे घण्टे में सहज ही और व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से कर सकेंगे। यह योग की क्रिया है। आप एक पूर्ण योगी बन जायेंगे । यहाँ तक कि जब आप अध्ययन करें, तो भी विषय को पूर्ण एकाग्रता के साथ पढ़ें। मन को भटकने न दें। आपको सभी बाह्य ध्वनियों को सुनना बन्द करना होगा। दृष्टि को एक बिन्दु पर टिकायें। आँखों को इधर-उधर न घूमने दें। जब आप एक विषय का अध्ययन करें, तो रेडियो या मिठाई अथवा मित्र के बारे में न सोचें। आपके लिए उस समय के लिए सम्पूर्ण जगत् मृत हो जाना चाहिए। धारणा की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए। कुछ स्थिर और निरन्तर अभ्यास के पश्चात् आप ऐसा कर सकेंगे। परेशान न हों। हताश न हों। कुछ समय लग सकता है। शान्तिपूर्वक और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। रोम एक दिन में नहीं बना। एक दिन के लिए भी अभ्यास न छोड़ें, चाहे आप बीमार ही क्यों न हों। आपकी असफलता में आपकी सफलता और आपकी दुर्बलता में आपकी शक्ति सन्निहित है। आगे बढ़ें। कमर कस लें। साहसी बनें। कोई हताशा नहीं । साहस के साथ आगे बढ़ें। उत्साहित रहें। ज्योतिर्मय भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अभ्यास करें। अनुभव करें। आनन्द लें। एक योगी अथवा महान् व्यक्तित्व बनें। मैं आपको ऐसा बनाऊँगा। मेरा अनुकरण करें। लगनशील एवं गम्भीर बनें। उठिए ! जाग जाइए। आपकी ज्योति आ गयी है। हे प्रकाश और अमरता के मेरे पुत्र, ब्राह्ममुहूर्त हो गया है, प्रातः के ३.३० बज गये हैं। यह आत्मा, स्मृति, संकल्प पर धारणा करने तथा मन को पकड़ने का समय है। वीरासन में बैठ जायें और कठोर साधना प्रारम्भ कर दें। आपको सफलता और कीर्ति प्राप्त हों! मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। मैं आपको यहाँ छोड़ दूँगा। मन के बुलबुले को ब्रह्मज्ञान के सागर में विलीन कर दें। परमानन्द का उपभोग करें।
७. अनाहत ध्वनियों पर धारणा
किसी आन्तरिक अथवा बाह्य विषय अथवा अनाहत ध्वनियों अथवा किसी असम्बद्ध विचार पर तीव्र और पूर्ण एकाग्रता जिसके साथ बाह्य विश्व अथवा इन्द्रियों जगत् से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु से प्रत्याहार भी सम्मिलित हो, धारणा कहलाती है।
साधना हेतु अभ्यास
पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जायें। कानों को अँगूठों से बन्द करके योनि मुद्रा का अभ्यास करें। दाहिने कान से आने वाली ध्वनि (वह ध्वनि जो आपको सभी बाह्य ध्वनियों के प्रति बहरा बना देगी) को सुनने का प्रयास करें। सभी बाधाओं पर विजय पा कर आप १५ दिन के भीतर तुरीयावस्था में प्रवेश करेंगे। अभ्यास के प्रारम्भ में आपको अनेक तीव्र ध्वनियाँ सुनायी देंगी। वे धीरे-धीरे तीव्र और अधिक तीव्र होती जायेंगी और अधिकाधिक सूक्ष्मतर सुनायी देंगी। आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करना है। आप अपना ध्यान सूक्ष्म से स्थूल की ओर परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने मन को उनकी ओर से अन्य विषयों की ओर नहीं मुड़ने देना है।
मन प्रारम्भ में स्वयं ही किसी एक ध्वनि पर दृढ़ता से टिक जाता है और इसमें विलीन हो जाता है। मन बाह्य प्रभावों के प्रति निष्प्रभावी हो जाता है और ध्वनि के साथ उसी प्रकार एक हो जाता है जैसे दूध के साथ पानी और यह चिदाकाश में गहरे लीन हो जाता है। सभी विषयों से निरपेक्ष रह कर तथा वासनाओं पर नियन्त्रण करके आपको निरन्तर अभ्यास के द्वारा अपने ध्यान को उस ध्वनि पर लगाना चाहिए जो मन को नष्ट कर देती है। सभी विचारों को त्याग कर और सभी कर्मों से मुक्त हो कर आपको अपना ध्यान ध्वनि पर एकाग्र करना चाहिए और तब आपका चित्त इसमें लीन होगा। जिस प्रकार जो मधुमक्खी मधु का पान करती है, वह गन्ध की चिन्ता नहीं करती; उसी प्रकार वह चित्त जो सदा ध्वनि में लीन है, वह विषयों की कामना नहीं करता, क्योंकि यह नाद की मधुर गन्ध से बँधा रहता है और इसने अपनी चिपकने वाली प्रकृति को त्याग दिया है । चित्त-सर्प नाद को सुन कर पूर्णतया इसमें लीन हो जाता है और प्रत्येक चीज़ के प्रति अचेतन रह कर स्वयं ही ध्वनि पर केन्द्रित हो जाता है। ध्वनि चित्त रूपी पागल हाथी जो कि विषय-वस्तुओं के सुन्दर बगीचे में घूम रहा है, को नियन्त्रित करने के लिए अंकुश का काम करता है।
यह चित्त-रूपी हिरण को बाँधने के लिए भाले की भाँति काम करता है। यह चित्त-रूपी समुद्र के लिए किनारों का काम करता है। प्रणव से निकलने वाला नाद जो कि ब्रह्म है, वह ज्योति स्वरूप प्रकृति का है, मन इसमें लीन हो जाता है। यह विष्णु भगवान् का परम धाम है। मन का तब तक अस्तित्व है, जब तक नाद हैं; लेकिन इसकी समाप्ति के बाद जो अवस्था होती है, उसे तुरीयावस्था कहते हैं। यह ध्वनि ब्रह्म में विलीन हो जाती है और ध्वनि रहित यह अवस्था परमावस्था है। नाद के ऊपर निरन्तर धारणा के द्वारा मन इसकी कार्मिक प्रवृत्तियों सहित नष्ट हो कर प्रणव के साथ ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। सभी अवस्थाओं और विचारों से मुक्त हो कर आप मृत समान हो जाते हैं। आप मुक्त बन जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। शरीर निस्सन्देह एक लकड़ी की भाँति हो जाता है और इसे सर्दी या गर्मी, सुख या दुःख का कोई अनुभव नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि जब कोई विषय न दिखायी दे, तब भी स्थिर हो जाती है। जब प्रणव बिना किसी प्रयत्न के स्थिर हो जाता है, तब चित्त बिना किसी अवलम्बन के दृढ़ हो जाता है, तब आप ब्रह्म बन जाते हैं (ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति)।
आप गुरु-दीक्षा द्वारा प्रथम नौ ध्वनियों को सुने बिना ही दसवीं ध्वनि सुन सकते हैं। प्रथम अवस्था में शरीर चिन चिनी बनता है, द्वितीय अवस्था में शरीर में भंजन (टूटन अथवा शरीर पर प्रभाव) होता है। तृतीयावस्था में भेदन होता है। चतुर्थ में सिर में कम्पन होता है। पंचम अवस्था में जिह्वा से लार बहने लगती है। षष्ठम अवस्था में अमृत प्राप्त होता है। सप्तम अवस्था में जगत् की गुप्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अष्टम अवस्था में परावाक् सुनायी देती है। नवम अवस्था में शरीर अभेद्य हो जाता है और दिव्य चक्षु विकसित हो जाते हैं। दशम अवस्था में आप परब्रह्म की अवस्था प्राप्त करते हैं। जब मन नष्ट हो जाता है, जब गुण और पाप नष्ट हो जाते हैं, आप ज्योतिर्मय, शुद्ध, अनन्त, निर्दोष, शुद्ध ब्रह्म की भाँति दमकने लगते हैं।
८. त्राटक
त्राटक स्थिर दृष्टि से देखना है। दीवार पर काले रंग से ॐ लिख लें। इस चित्र के सामने बैठ जायें। इसको तब तक खुली आँखों से देखें, जब तक कि आँखों से आँसू न बहने लगें। तत्पश्चात् आँखें बन्द कर लें। ॐ को देखने का प्रयास करें। फिर आँखें खोल लें और तब तक एकटक देखते रहें, जब तक आँसू न बहने लगें। इस समयावधि में धीरे-धीरे वृद्धि करें। कई ऐसे अभ्यासी हैं जो एक घण्टे तक त्राटक कर सकते हैं। त्राटक हठयोग की षटक्रियाओं में से एक है। ॐ का चित्र ले आयें, इसे दीवार पर लगा दें। इस पर धारणा करें। यह चित्र बाजार में मिलता है। त्राटक से घुमन्तु मन स्थिर होता है। यह विक्षेप दूर करता है। ॐ पर त्राटक करने के स्थान पर आप दीवार पर एक बड़े काले बिन्दु पर भी त्राटक कर सकते हैं। अथवा आप एक सफेद कागज पर एक बड़ा काला बिन्दु बना लें और इसे दीवार पर चिपका लें। इस बिन्दु पर त्राटक करें। यह योग के विद्यार्थी के लिए अपने मन की धारणा करने के लिए लक्ष्य होगा। त्राटक करते समय दीवार स्वर्णिम रंग की दिखायी देगी।
आप भगवान् के किसी भी चित्र पर जैसे कृष्ण, राम, शिव आदि के चित्र पर अथवा शालग्राम पर त्राटक कर सकते हैं। आप कुर्सी पर बैठ कर अपनी आँखों के सामने दीवार पर चित्र लगा कर उसके ऊपर त्राटक कर सकते हैं। त्राटक धारणा की वर्णमाला का प्रथम अक्षर है। यह योग के विद्यार्थियों के लिए धारणा का प्रथम चरण है। खुली आँखों से त्राटक करने से मन में विषय का चित्र बनता है। त्राटक तथा मानसिक परिकल्पना धारणा में बहुत सहायता करते हैं।
मानसिक पूजा करने से, ईश्वर के गुणों का चिन्तन करने से तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करने से भी मन स्थिर होता है।
प्रथम दिन एक मिनट तक त्राटक करें। इसके बाद प्रत्येक सप्ताह धीरे-धीरे समय में वृद्धि करें। आँखों पर जोर न डालें। त्राटक को जितनी देर तक सम्भव हो, आराम से और सहजता से करें। त्राटक करते समय अपने इष्टमन्त्र, हरि ॐ, श्री राम अथवा गायत्री मन्त्र का जप करें। कुछ लोगों की आँखों की रक्त नलिकाएँ दुर्बल होती हैं, इसलिए आँखें लाल हो जाती है। उनको अनावश्यक रूप से चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही आँखों की लाली लुप्त हो जायेगी। त्राटक का अभ्यास छह माह तक करें। इसके पश्चात् आप धारणा और ध्यान की उच्च साधना करें। अपनी साधना को नियमित और क्रमबद्ध रूप से करते रहें। यदि किसी कारण से क्रम टूट जाये, तो अगले दिन उस कमी को पूरा करें। त्राटक अनेक नेत्र रोगों का उन्मूलन करता है और अन्त में सिद्धियाँ प्रदान करता है।
अध्याय ३
ध्यान हेतु पूर्वापेक्षाएँ
१. ध्यान क्या है?
'ध्यानं निर्विषयं मनः " मन की वह स्थिति जहाँ ध्यान में कोई विषय अथवा विषय के विचार नहीं होते।
"तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ” – दृष्टि अथवा विचार का निरन्तर प्रवाह ध्यान कहलाता है। जैसे नदी में जल का प्रवाह होता है, उसी प्रकार ध्यान में एक विषय का निरन्तर प्रवाह होता है। इसमें मन में एक ही वृत्ति होती है। वह वृत्ति है एकरूप - वृत्ति - प्रवाह ।
ईश्वरीय चेतना के निरन्तर प्रवाह को बनाये रखना ध्यान है। यह एक वस्तु अथवा ईश्वर अथवा आत्मा का तैलधारावत् निरन्तर प्रवाह है। इसमें सभी सांसारिक विचार मन में आना बन्द हो जाते हैं। मन दैवी विचारों से, दैवी वैभव से, दैवी उपस्थिति से परिपूर्ण अथवा सन्तुष्ट रहता है। ध्यान धारणा के विषय से सम्बन्धित विचारों का नियमित प्रवाह है। ध्यान धारणा का अनुगामी है।
ध्यान योग की सातवीं सीढ़ी है। योगी इसे 'ध्यान' कहते हैं। ज्ञानी इसे 'निदिध्यासन' कहते हैं। भक्त इसे 'भजन' कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये योग के आठ चरण हैं।
प्रभु यीशु कहते हैं- “स्वयं को रिक्त कर दो, मैं तुम्हें भर दूँगा।" यह पतंजलि महर्षि के उस कथन के समान है, वे कहते हैं: “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ” – सभी चित्तवृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। यह रिक्त करने की क्रिया-विधि निस्सन्देह अत्यन्त कठिन है; लेकिन निरन्तर कठोर अभ्यास से सफलता मिलती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।
२. ध्यान की आवश्यकता
अमरता और अनन्त आनन्द की प्राप्ति हेतु ध्यान एकमात्र मार्ग है। ईशावास्य उपनिषद् के तीसरे मन्त्र में लिखा है- "जो धारणा और ध्यान नहीं करते, वे वास्तव में आत्मा को मारने वाले (आत्महनः) हैं। वे जीवित शव के समान और अभागे नीच हैं।"
ज्ञानी अहंकार की ग्रन्थि को निरन्तर ध्यान की तलवार से काट देते हैं। तब मुक्त योगी को अब न तो सन्देह होता है और न ही भ्रम। कर्मों के सभी बन्धन अब कट जाते हैं। इसलिए सदा ध्यान में लगे रहो। यह स्थायी आनन्द के प्रदेश को खोलने की चाबी है।
प्रारम्भ में यह अवश्य ही थका देने वाला और उबाऊ लगेगा, क्योंकि मन धारणा के बिन्दु से प्रति क्षण भागता है। कुछ अभ्यास के बाद में यह केन्द्र में केन्द्रित हो जायेगा और आप दैवी आनन्द में लीन हो जायेंगे।
प्राचीन काल के महान ऋषि गण जैसे याज्ञवल्क्य, उद्दालक आदि ने प्रबल ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया जो कि परम ऐक्य को सुरक्षित करने हेतु साधन है।
जिस प्रकार आपको शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को प्रार्थना, जप, कीर्तन, ध्यान आदि के रूप में भोजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जब आपको सही समय पर भोजन नहीं मिलता, तो आप उत्तेजित हो जाते हैं; उसी प्रकार यदि आप कुछ समय तक प्रार्थना और जप का अभ्यास करेंगे और यदि किसी कारणवश आपने प्रातः काल और सायंकाल प्रार्थना नहीं की, तो आप उत्तेजित हो जायेंगे। आत्मा का भोजन शरीर के भोजन से अधिक आवश्यक है। इसलिए अपनी प्रार्थना, जप और ध्यान नियमित रूप से करें।
जिस प्रकार आप अपने बगीचे में गुलाब, चमेली और लिली आदि के पुष्प लगाते हैं, उसी प्रकार आपको अपने अन्तःकरण के बृहत् बगीचे में शान्तिपूर्ण विचारों, प्रेम, करुणा, दया, शुद्धता आदि के विचारों के पुष्पों को लगाना चाहिए। अन्तरावलोकन के द्वारा आपको मन के बगीचे को जल से सींचना चाहिए तथा ध्यान और उत्कृष्ट चिन्तन के द्वारा निरर्थक, निरुपयोगी, नष्ट करने योग्य विचारों की खरपतवार का उन्मूलन करें।
जब आप अपने आम के वृक्ष के ऊपर बौर देखते हैं, तो आपको यह भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि आपको शीघ्र ही आम प्राप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार जब आपके मन में शान्ति आये, तो यह निश्चित मानें कि आपका शीघ्र ही अच्छा ध्यान लगने लगेगा और आपको शीघ्र ही ज्ञान रूपी फल प्राप्त होगा।
जो चीजें एक जैसी होती हैं, वे एक-दूसरे को आकर्षित करती हैं। यह एक महान् सिद्धान्त है। उत्तम विचारों का पोषण करें। ध्यान करें। आप सन्तों, योगियों तथा सिद्धों को आकर्षित करेंगे। आप उनके स्पन्दनों से लाभान्वित होंगे। आपके नवीन आध्यात्मिक स्पन्दन उनको आकर्षित करेंगे।
३. ध्यान का फल
वह सन्त जिसका मन कामनाओं से मुक्त तथा आत्म-केन्द्रित है, जो अपने आत्म-स्वरूप में स्थित है तथा जिसके पास सभी के प्रति समदृष्टि है, उसे जो आनद प्राप्त होता है, वह देवताओं एवं प्रचुर सम्पदा के स्वामी इन्द्र को भी दुर्लभ है।
आत्म-नियन्त्रण की विद्या को सीखिए। निरन्तर ध्यान के अभ्यास से मन को स्थिर रखिए। अपने मन को ईश्वर में लगाइए। आपको दिव्य जीवन प्राप्त होगा। ज्ञान का प्रकाश ज्योतित होगा। आपके भीतर सभी दैवी गुण का प्रवाह होगा। सभी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जायेंगी। सभी विरोधी बल अनुकूल हो जायेंगे। आप पूर्ण सामंजस्य, निर्विघ्न आनन्द, आन्तरिक शान्ति का उपभोग करेंगे।
ध्यान मोक्ष की प्राप्ति हेतु एकमात्र सच्चा और राज मार्ग है। ध्यान सभी दुःखों, कष्टों का नाश करता है। ध्यान दुःखों के सभी कारणों का नाश करता है। ध्यान समदृष्टि प्रदान करता है। ध्यान ईश्वर से मिलन के अनुभव को प्रेरित करता है। ध्यान एक गुब्बारा अथवा हवाई जहाज के समान है, जो साधक को अनन्त आनन्द, स्थायी शान्ति और अक्षय आनन्द के लोक में ऊँचे उड़ने में सहायता करता है।
ध्यान देवत्व प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो साधक को दैवी चेतना के लक्ष्य तक सीधे ले कर जाता है। यह एक रहस्यमय सीढ़ी है, जो योगाभ्यासी को धरती से स्वर्ग तक ले कर जाती है। यह योगियों की दिव्य सीढ़ी है, जो उन्हें असम्प्रज्ञात समाधि की ऊँचाइयों तक उठाती है। यह साधक को अद्वैत निष्ठा की सर्वोच्च मंजिल तक एवं वेदान्तियों की कैवल्य मुक्ति तक ले जाने के लिए चिदाकाश की सीढ़ी है। बिना इसके किंचित् भी आध्यात्मिक प्रगति सम्भव नहीं है। यह वह मार्ग है, जो भक्त को भाव समाधि के दूसरे किनारे तक सरलता से पहुँचाने में तथा प्रेम का मधु और अमरता का अमृत पीने हेतु सहायता करता है।
नियमित ध्यान अन्तर्ज्ञान के द्वार खोलता है, मन को शान्त और स्थिर बनाता है। यह समाधि के अनुभव को जाग्रत करता है तथा योगाभ्यासी को परम पुरुष के स्रोत के सम्पर्क में ले कर आता है। यदि कोई सन्देह रहता है, तो जब आप ध्यान के पथ पर स्थिर चलते हैं, तो वह स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। आपको स्वयं ही आध्यात्मिक सीढ़ी पर अपने पैर रखने के मार्ग का अनुभव होता है। एक रहस्यमय आन्तरिक वाणी आपका निर्देशन करती है। इसे ध्यान से सुनो, हे योगीन्द्र ।
यदि आप घड़ी को रात के समय ध्यान से देखेंगे, तो आप पायेंगे कि यह चौबीसों घण्टे सहज रूप से चलती रहती है। इसी प्रकार यदि आप प्रातः ब्राह्ममुहूर्त में एक अथवा दो घण्टे ध्यान करें, तो आप सारे दिन शान्तिपूर्ण ढंग से कार्य कर सकेंगे। कोई भी बात आपके मन को विचलित नहीं कर सकेगी। आपका सम्पूर्ण शरीर आध्यात्मिक स्पन्दनों अथवा दैवी लहरों से आवेशित हो जायेगा।
ध्यान के समय आपके सन्देहों का स्वयं ही निराकरण हो जायेगा। कुछ लोगों को उनके सन्देहों का निराकरण करने के लिए कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कितना भी कोई शिक्षक समझाये, परन्तु कुछ बातें एक ही समय पर समझ में नहीं आतीं। आपको थोड़ा और विकसित होना होगा। जब आप विकसित हो जायेंगे, तो वे सन्देह जो आपको तीन वर्ष पूर्व परेशान करते थे, वे अब स्पष्ट हो जायेंगे।
जब आपको अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है अथवा जब आपको बड़ा फोड़ा होता है, तो आपको अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है; किन्तु नींद में आपको तनिक भी दर्द का अनुभव नहीं होता। जब आप क्लोरोफार्म सूँघ लेते हैं, तो भी दर्द नहीं होता।
आत्मा आनन्दघन है। यदि आप मन को शरीर और विषयों से खींच लें और इसे निरन्तर ध्यान के द्वारा आत्मा पर केन्द्रित करें, तो सभी दर्द समाप्त हो जायेंगे। ध्यान सभी मानवीय दुःखों को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इसके सिवा इनसे मुक्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है।
ध्यान के समय जब मन आत्मा में विश्राम करता है, तो सच्चा विश्राम मिलता है। कार्य का परिवर्तन भी विश्राम प्रदान कर सकता है। बिना किसी काम के आलसी बने रहने और मन को उन्मत्त हाथी की भाँति जंगली की तरह घूमने देने और हवाई किले बनाने से विश्राम नहीं मिलता।
वह व्यक्ति जो ध्यान में अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता है, उसे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। अस्थिर मन किसी प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता। उसे आत्मज्ञान के प्रति किसी प्रकार का समर्पण अथवा मोक्ष के प्रति कोई ज्वलन्त आकांक्षा नहीं होती। वह जो किसी प्रकार का ध्यान नहीं करता, उसके पास मन की शान्ति नहीं होती। अशान्तिपूर्ण व्यक्ति के लिए खुशी कहाँ हो सकती है?
धीरे से आपको स्वप्न में भी नियन्त्रण का अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिए। जब यह मन कुछ गलत करे, तो आपको मन को रोकना चाहिए। जब आप निद्रा में होंगे, तो आपकी सहायता के लिए आयेगा। यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। स्वप्न को सावधानीपूर्वक देखें।
यह संसार दुःखों और कष्टों परिपूर्ण है। यदि आप इस संसार के दुःखों और कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान दिव्यता का पथ है। यह ब्रह्मधाम का राज मार्ग है। यह एक रहस्यमय सीढ़ी है जो धरती से स्वर्ग (वैकुण्ठ, कैलास अथवा ब्रह्मलोक) तक, असत्य से सत्य तक, अन्धकार से प्रकाश तक, दुःख से आनन्द तक, बेचैनी से आनन्द के धाम तक, अज्ञानता से ज्ञान तक, मर्त्यता से अमरता तक पहुँचती है। ध्यान आत्मज्ञान तक ले कर जाता है, जो अनन्त शान्ति और परमानन्द लाता है। ध्यान आपको सम्पूर्ण अनुभव तथा प्रत्यक्ष अन्तर्ज्ञान हेतु तैयार करता है।
सत्य ही ब्रह्म है। सत्य ही आत्मा है। सत्य पूर्ण शुद्ध और सरल है। बिना ध्यान के आप सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। शान्त रहें। स्वयं को जानें। उसे जानें। मन को उसमें द्रवीभूत कर दें।
ध्यान के बिना आप आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। बिना इस सहायता के आप दैवी अवस्था तक विकास नहीं कर सकते। आप मन के जंजाल से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते, अमरता नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आप ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं, तो आत्मा का परम वैभव एवं सदाबहार सौन्दर्य आपसे छिपा रहेगा। नियमित ध्यान के अभ्यास से आत्मा को ढाँकने वाले आवरण को चीर दीजिए। आत्मा को जिन पाँच कोशों ने ढाँक रखा है, उनको निरन्तर ध्यान से छिन्न-भिन्न कर दीजिए और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कीजिए ।
ध्यान की अग्नि दुर्गुणों से होने वाली समस्त हानियों का उन्मूलन करती है। तब अचानक ज्ञान अथवा दैवी ज्ञान आता है, जो सीधे मुक्ति अथवा अन्तिम मोक्ष तक ले कर जाता है।
मन के प्रशिक्षण के अनेक प्रकार हैं, जो मानसिक शक्तियों के विकास के लिए अनिवार्य हैं—जैसे उदाहरण के लिए स्मरण शक्ति का प्रशिक्षण, ध्यान का अर्जन, विवेक, विचार अथवा 'मैं कौन हूँ' की खोज। ध्यान का अभ्यास स्वयं ही स्मृति का. शोधक है। स्मरण-शक्ति में वृद्धि का प्रशिक्षण ध्यान-प्राप्ति में अत्यन्त सहायक है।
ध्यान एक शक्तिशाली शक्तिवर्धक है। यह एक मानसिक तथा नाड़ी शक्तिवर्धक भी है। पवित्र स्पन्दन शरीर की सभी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर के रोगों का भी उपचार करते हैं। जो ध्यान करते हैं, उनका डाक्टरों का बिल बचता है। ध्यान के समय उत्पन्न होने वाली शक्तिशाली तथा शान्तिपूर्ण तरंगें मन, नाड़ियों, अंगों तथा कोशिकाओं के ऊपर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव डालती हैं। ईश्वर के चरणों से दैवी ऊर्जा तैलधारावत् साधक के विभिन्न अंगों की ओर प्रवाहित होती है।
यदि आप आधा घण्टे तक ध्यान कर सकते हैं, तो ध्यान के बल पर जीवन के संघर्ष में आप शान्तिपूर्वक एवं आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक सप्ताह तक कार्य कर सकते हैं। ध्यान का ऐसा लाभदायक प्रभाव है। चूँकि आपको अपने दैनिक जीवन में विशिष्ट प्रकृति वाले विभिन्न मनों के साथ चलना पड़ता है, इसलिए ध्यान से शक्ति और शान्ति प्राप्त कीजिए और तब आपको किसी प्रकार का कष्ट और चिन्ता नहीं होगी।
वह योगी जो नियमित ध्यान करता है, उसका व्यक्तित्व चुम्बकीय और आकर्षक होता है। जो उसके सम्पर्क में आते हैं, उनकी वाणी मधुर और शक्तिशाली भाषण, तेजस्वी नेत्र, चमकदार रंग, बलवान् और स्वस्थ शरीर, उत्तम व्यवहार, सद्गुणों तथा दिव्य प्रकृति से प्रभावित रहते हैं। जिस प्रकार नमक का एक कण जल के बर्तन में गिरने पर सारे जल में घुल कर एक हो जाता है, जिस प्रकार चमेली के फूल की सुगन्ध वायु में सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार योगी का आध्यात्मिक आभा-मण्डल अन्यों के मन में प्रविष्ट हो जाता है। लोग उससे आनन्द, शान्ति और शक्ति प्राप्त करते हैं। वे उसके भाषणों से प्रभावित होते हैं और उसके सम्पर्कमात्र से ही मन का उत्थान करते हैं।
ध्यान अन्तर्ज्ञान तथा अनेक शक्तियों हेतु मन के द्वार खोलता है।
ध्यान करें ! ध्यान करें! एक क्षण भी न गँवायें। ध्यान जीवन के सभी दुःखों का उन्मूलन कर देगा। यही एकमात्र मार्ग है। ध्यान मन का शत्रु है। यह मनोनाश लाता है।
वह महात्मा जो हिमालय की एकान्त गुहा में ध्यान करता है, वह अपने आध्यात्मिक स्पन्दनों द्वारा इस जगत् की उस साधु की अपेक्षा अधिक सहायता करता है, जो मंच पर ध्यान करना सिखाता है। जिस प्रकार ध्वनि की तरंगें आकाश में चलती हैं, उसी प्रकार एक ध्यान करने वाले की आध्यात्मिक तरंगें बड़ी लम्बी दूरी तक जाती हैं और हजारों लोगों को शान्ति तथा शक्ति प्रदान करती हैं।
जब ध्यानाभ्यासी मन रहित हो जाता है, तो वह सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त तथा प्रविष्ट हो जाता है। अज्ञानी लोग यह दोषारोपण करते हैं कि वह साधु जो गुफा में ध्यान करता है, वह स्वार्थी है।
नियमित ध्यान के द्वारा अपने चारों ओर एक दृढ़ किले का तथा चुम्बकीय आभा मण्डल का निर्माण कीजिए, जो माया के सन्देशवाहकों द्वारा भी न भेदा जा सके।
शुद्धता के उपरान्त ईश्वर पर मन की धारणा आपको सच्ची प्रसन्नता और ज्ञान प्रदान करेगी। राग और मोह के द्वारा आप बाह्य विषयों की ओर खींचे जाते हैं। गहरे उतरें। अपने भीतर लीन हो जायें।
ध्यान के समय जब आपका मन अधिक सात्त्विक रहता है, तो आपको अन्तः प्रेरणा होने लगेगी। मन अच्छी कविताओं की रचना करेगा और आप जीवन की समस्त समस्याएँ हल करने लगेंगे। इन सात्त्विक वृत्तियों को भी चूर-चूर कर दें। यह सब मानसिक ऊर्जा का विकिरण है। मात्र आत्मा में ही ऊंचे ही ऊंचे जायें।
आपको दिव्यता का पूर्ण आनन्द मात्र तभी प्राप्त होगा, जब आप गहरे गोते लगायेंगे, जब आप शान्त ध्यान में गहरे लीन हो जायेंगे। जब तक आप प्रभु की दिव्यता के सीमावर्ती प्रदेश पर होंगे, जब तक आप ईश्वर की देहली अथवा द्वार पर होंगे, जब तक आप बाहरी सीमा पर होंगे, आपको परम शान्ति और परम आनन्द नहीं प्राप्त होगा।
ध्यान के समय कुछ दृश्यों में आप स्वयं के विचारों का भौतिकीकरण देखेंगे, जब कि अन्य दृश्य सत्य और तथ्यपरक होंगे।
सच्ची शान्ति और आनन्द मात्र तभी प्रकट होगा, जब वासनाएँ तनु हो जाती हैं और संकल्प नष्ट हो जाते हैं। जब आप मन को भगवान् श्री कृष्ण, शिव अथवा आत्मा पर यदि पाँच मिनट के लिए भी एकाग्र करते हैं, तो सत्त्व गुण मन में प्रवेश कर जाता है। वासनाएँ तनु हो जाती हैं। इन पाँच मिनटों में आप शान्ति और आनन्द का अनुभव करेंगे। आप सूक्ष्म बुद्धि के साथ इस ध्यान के द्वारा प्राप्त आनन्द की क्षणिक विषयी आनन्द से तुलना कर सकते हैं। आप इस ध्यान से प्राप्त आनन्द को विषयी आनन्द से करोड़ों गुना श्रेष्ठ पायेंगे। ध्यान करें और इस आनन्द का अनुभव करें। तभी आप सच्चा मूल्य जानेंगे।
यदि कश्मीर में एक साधक अपने गुरु का उत्तरकाशी में ध्यान करता है, तो उसके तथा गुरु के मध्य एक निश्चित सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। गुरु साधक के विचारों के प्रत्युत्तर में उसे शक्ति, शान्ति और आनन्द विकिरित करता है। वह शक्तिशाली चुम्बकीय तरंगों में स्नान करता है। आध्यात्मिक विद्युत् का प्रवाह गुरु से शिष्य की ओर धीरे-धीरे उसी प्रकार होता रहता है, जिस प्रकार तेल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में निरन्तर प्रवाहित होता रहता है। शिष्य अपने गुरु से अपनी आस्था के अनुरूप ग्रहण करता है। जब शिष्य अपने गुरु के ऊपर गम्भीरता से ध्यान करता है, तो गुरु को वास्तव में ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उसके शिष्य से निकलने वाली प्रार्थना अथवा उत्कृष्ट विचार की तरंगें उसके हृदय को स्पर्श कर रही हैं। जिसकी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि होती है, वह गुरु और शिष्य के मध्य एक चमकदार प्रकाश की रेखा जो कि चित्त के समुद्र में सात्त्विक विचारों के कारण बनती है, को देख सकता है।
ज्ञान का अचानक स्पर्श अनुभवाश्रित अस्तित्व को भी समाप्त कर देता है तथा संसार जैसी चीज की स्मृति अथवा आत्मा की संकीर्ण वैयक्तिकता के विचार भी उसे पूर्णतया त्याग देते हैं।
जब योगी ध्यान तथा समाधि की अन्तिम अवस्था में पहुँचता है, उसके कर्मों के अन्तिम अवशेष पूर्णतया दग्ध हो जाते हैं। वह इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह जीवन्मुक्त होता है।
ध्यान अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति, शान्ति, नवीन ऊर्जा तथा जीवनी शक्ति प्रदान करता है। यह सर्वश्रेष्ठ मानसिक शक्तिवर्धक है। यदि ध्यान करने वाला अक्सर क्रोधित हो उठता है, तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि वह निर्विघ्न ध्यान नहीं कर रहा है। उसकी साधना में कुछ-न-कुछ दोष अवश्य है।
ध्यान दृढ़ और शुद्ध विचारों का विकास करता है। इसके अभ्यास से मानसिक प्रतिबिम्ब अत्यन्त स्पष्ट होते हैं। अच्छे विचार दृढ़ होते हैं। विचारों के स्पष्टीकरण के द्वारा भ्रम समाप्त हो जाता है।
जिस प्रकार एक अगरबत्ती से निरन्तर सुगन्धि निकलती रहती है, उसी प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक के मुख-मण्डल से निरन्तर सुगन्धि तथा दिव्य तेज (ब्रह्मवर्चस्, ब्रह्मतेज से युक्त आभा-मण्डल) निरन्तर निकलता रहता है। जो ध्यानाभ्यास करते हैं, उनका मुख मण्डल शान्त और आकर्षक, मधुर वाणी तथा नेत्रों में तेज होता है।
जिस प्रकार एक बंजर भूमि में कृषि करने से कोई लाभ नहीं है, उसी प्रकार बिना वैराग्य के किया गया ध्यान निष्फल रहता है।
यदि आप आधा घण्टे नित्य ध्यान करते हैं, तो ध्यान की शक्ति और बल से आप नित्य दैनिक जीवन के संग्राम में शान्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक सप्ताह तक लगे रह सकते हैं। ध्यान की अग्नि दुर्गुणों के सभी प्रभावों को दग्ध कर देती है। तब अचानक दिव्य ज्ञान आता है जो सीधे मुक्ति अथवा मोक्ष प्रदान करता है।
ध्यान में आप अपरिवर्तनीय प्रकाश के आध्यात्मिक सम्पर्क में रहते हैं। आपकी सभी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं।
यह प्रकाश उस आत्मा को स्वच्छ कर देता है जो इसके सम्पर्क में रहती है। लैंस को सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है, उसके नीचे जो तृण रहते हैं, वे आग पकड़ लेते हैं। इसलिए आपके भीतर यदि एक खुला हृदय है जो कि पूर्णरूपेण ईश्वर के प्रति समर्पित है, उनकी पवित्रता और प्रेम का प्रकाश इस खुली आत्मा को प्रकाशमान करता है और यह दैवी प्रेम की अग्नि आपकी सभी कमियों को जला डालती है। यह प्रकाश अत्यधिक शक्ति तथा सुख ले कर आता है।
सभी दृश्यमान वस्तुएँ माया हैं। ज्ञान के द्वारा अथवा आत्मा पर ध्यान के द्वारा माया नष्ट हो जाती है। व्यक्ति को माया से स्वयं को मुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। माया मन के द्वारा विनाश करती है। मन के नाश का अर्थ है माया का उन्मूलन कर देना। निदिध्यासन (आत्मा पर ध्यान) माया को विजित करने का मार्ग है। भगवान् बुद्ध, राजा भर्तृहरि, दत्तात्रेय, गुजरात के अखो—सभी ने माया और मन को मात्र गहन ध्यान के द्वारा विजित किया था। एकान्त में प्रवेश करें और ध्यान करें।
जो ध्यानाभ्यास करते हैं, वे पाते हैं कि वे उन लोगों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील हैं, जो ध्यान नहीं करते और इस कारण उनके भौतिक शरीर पर अत्यधिक खिंचाव रहता है। कभी-कभी उच्च साधक सोचने लगते हैं कि भगवद्-साक्षात्कार की स्थिति कैसी होगी? भगवान् मेरे सामने कैसे प्रकट होंगे? वे मुझे किस प्रकार दर्शन देंगे? भगवद्-साक्षात्कार वर्णन के परे है। इसका वर्णन करना सम्भव नहीं है। इसका वर्णन करने का कोई साधन नहीं है। वहाँ पूर्ण शान्ति है, वहाँ अवर्णनीय आनन्द है। वहाँ पूर्ण एकान्त है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है। मन, बुद्धि तथा इन्द्रियाँ कार्य करना बन्द कर देती हैं। वहाँ अन्तर्ज्ञानात्मक अनुभव होता है। मात्र इतना ही कहा जा सकता है। आपको समाधि में स्वयं ही इसे अनुभव करना होगा।
नियमित ध्यान के अभ्यास से मन का भटकना रुक जायेगा। ध्यान चिड़चिड़ाहट दूर करता है और तदनुरूप मन की शान्ति को प्रेरित करता है।
४. ब्राह्ममुहूर्त - -ध्यान हेतु सर्वश्रेष्ठ समय
हे साधको! ब्राह्ममुहूर्त में उठ बैठो और ध्यान का अभ्यास करो। इसमें किसी भी मूल्य पर असफल न हों। प्रातः ३.३० से ५.५० बजे तक का समय ब्राह्ममुहूर्त कहलाता है। यह ध्यान हेतु बड़ा ही अनुकूल है। अच्छी नींद के उपरान्त इस समय मन एकदम ताजा रहता है। मन इस समय शान्त और स्थिर रहता है। इस समय मन में सत्त्व अथवा शुद्धता की अधिकता रहती है। वातावरण में भी इस समय सत्त्व की अधिकता रहती है।
इस समय मन कोरे कागज की भाँति रहता है और तुलनात्मक रूप से सांसारिक संस्कारों अथवा प्रभावों से मुक्त रहता है। इस समय राग-द्वेष की तरंगें मन में गहराई से प्रविष्ट नहीं रहती हैं। इस समय जैसा आप चाहें, वैसा मन को मोड़ सकते हैं। अभी आप सरलता से मन को दैवी विचारों से आवेशित कर सकते हैं।
हिमालय के सभी योगी, परमहंस, संन्यासी जन, साधक और ऋषि इस समय अपना ध्यान प्रारम्भ करते हैं और समस्त जगत् को अपनी तरंगें भेजते हैं। आप उनकी आध्यात्मिक तरंगों से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। ध्यान स्वयं ही बिना किसी प्रयत्न के लग जायेगा। यदि आप इस समय सोते रहे और यदि आपने इस समय का उपयोग दैवी ध्यान में नहीं किया, तो आपका बहुत अधिक नुकसान हो जायेगा। कुम्भकर्ण न बनें। ज्ञानदेव की भाँति योगी बनें।
शीत ऋतु में आवश्यक नहीं कि आप शीतल जल से स्नान करें। मानसिक स्नान पर्याप्त होगा। कल्पना करें और अनुभव करें कि 'मैं प्रयाग में पवित्र त्रिवेणी अथवा बनारस में मणिकर्णिका में स्नान कर रहा हूँ।' शुद्ध आत्मा का स्मरण करें। इस सूत्र को दोहरायें—“मैं सदा पवित्र आत्मा हूँ।" यह ज्ञान गंगा में किया जाने वाला स्नान है। यह सर्वाधिक शक्तिशाली ज्ञान-स्नान है। यह अत्यधिक शुद्ध करने वाला है। यह समस्त पापों को दग्ध कर देता है। अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक नित्य शौचादि कर्म निबटा लें। दाँतों को शीघ्र स्वच्छ कर लें। दाँतों को साफ करने और स्नान करने में अधिक समय न गँवायें। जल्दी करें और शीघ्र तैयार हो जायें। ब्राह्ममुहूर्त शीघ्र समाप्त हो जायेगा। आपको इस बहुमूल्य समय का उपयोग जप तथा ध्यान में करना चाहिए।
मुँह, हाथ और पैरों को शीघ्रता से धो लें। मुख-मण्डल तथा सिर के शीर्ष भाग पर ठण्डा पानी छिड़कें। यह मस्तिष्क और नेत्रों को शीतल करेगा। सिद्ध, पद्म अथवा सुख आसन में बैठें। ब्रह्म की परम ऊँचाई, दैवी वैभव के शिखर पर पहुँचने का प्रयत्न करें।
यदि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो एक अलार्म घड़ी रखें। एक बार आदत पड़ गयी, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अवचेतन मस्तिष्क आपको विशेष समय पर जगाने के लिए आपका आज्ञाकारी दास बन जायेगा।
यदि आप जीर्ण कब्ज के शिकार हैं, तो आप दाँत साफ करते ही तुरन्त एक गिलास ठण्ढा अथवा गर्म जल पी सकते हैं। यह हठयोग का उषापान उपचार है। इससे आपका कब्ज दूर हो जायेगा। आप त्रिफला जल भी पी सकते हैं। दो हरड़, दो आँवले और दो बहेड़े रात के समय एक गिलास जल में भिगो दें। प्रातः काल दाँत साफ करने के बाद इस जल को पियें। आप इन तीनों का चूर्ण भी तैयार करके रख सकते हैं। यह चूर्ण एक या दो चम्मच एक गिलास जल में भिगो दें और सुबह इसे पी लें।
बिस्तर से उठते ही शीघ्र शौच हेतु जाने की आदत बना लें। यदि आप पुराने पाप के कारण असाध्य पुराने कब्ज रोग के शिकार हैं, तो प्रातः उठते ही शीघ्र ध्यानाभ्यास करें। आप ध्यान समाप्त होने के पश्चात् एक कप गर्म जल की सहायता से शौच हेतु जा सकते हैं।
जैसे ही आप बिस्तर से उठें, जप और ध्यान करें। यह महत्त्वपूर्ण है। ध्यान तथा जप समाप्त होने के पश्चात् आप आसन और प्राणायाम का अभ्यास एवं गीता तथा अन्य धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय कर सकते हैं।
प्रत्येक सन्ध्या का समय ध्यान हेतु अत्यन्त उपयोगी है। ब्राह्ममुहूर्त और सन्ध्या के समय सुषुम्ना नाड़ी सरलता से प्रवाहित होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित हो रही हो, उस समय आप गहन ध्यान और समाधि में बिना किसी प्रयत्न के प्रविष्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि ऋषि, योगी और शास्त्र – सभी ने इन दोनों सन्ध्याओं का बहुत अधिक महत्त्व बताया है। जब श्वास दोनों नासारन्ध्रों से प्रवाहित हो रही हो, तो जानें कि सुषुम्ना प्रवाहित हो रही है। जब भी सुषुम्ना कार्य कर रही हो, उस समय ध्यान हेतु बैठ जायें और आत्मा के आन्तरिक आनन्द का लाभ लें।
जप अथवा ध्यान प्रारम्भ करने के पूर्व दैवी स्तोत्रों तथा गुरु-स्तोत्र का पाठ या १२ बार ॐ का उच्चारण अथवा ५ मिनट तक कीर्तन करें। आप शीघ्र ही मन का उत्थान और आलस्य और नींद को दूर कर सकेंगे। शीर्षासन अथवा सर्वांगासन अथवा किसी भी आसन और प्राणायाम का अभ्यास ५-५ मिनट तक करें। यह आपको ध्यान हेतु तैयार कर देगा और निद्रा और आलस्य को दूर भगा देगा।
यह ब्राह्ममुहूर्त है! सोयें नहीं। बिस्तर में करवट न बदलें। कम्बल को फेंक दें। उठ जायें और अपना ध्यान प्रारम्भ कर दें तथा अन्तरात्मा के अनन्त आनन्द का अनुभव करें।
५. ध्यान-कक्ष
एक अलग ध्यान का कमरा रखें। इसे ताला लगा कर बन्द रखें। इसका प्रयोग एकान्त वन की भाँति करें। किसी को भी कमरे के भीतर प्रवेश न करने दें। इसे पवित्र रखें। यदि आप एक अलग कमरा न रख सकें, तो कमरे के एक छोटे से कोने को परदे लगा कर ध्यान के कमरे में बदल डालें। प्रातः काल तथा सायंकाल यहाँ अगरबत्ती और कर्पूर जलायें। भगवान् श्री कृष्ण, शिव, राम, देवी, गायत्री, गुरु, ईसामसीह अथवा बुद्ध भगवान् का चित्र रखें। अपना आसन चित्र के सामने रखें। कुछ पुस्तकें—जैसे गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद्, विवेकचूड़ामणि, योगवासिष्ठ, ब्रह्मसूत्र, बाइबिल, जेन्द अवस्ता, कुरान आदि भी कमरे में रखें।
कमरे को महान् सन्तों, ऋषियों, पैगम्बरों तथा जगद्गुरुओं के चित्रों से सजा कर रखें। कमरे में प्रवेश करने के पूर्व स्नान कर लें अथवा अपने मुख मण्डल, हाथों और पैरों को धो लें। देवता के समक्ष आसन के ऊपर बैठ जायें। भक्ति-स्तोत्रों अथवा गुरु-स्तोत्रों का पाठ करें। इसके पश्चात् जप, धारणा और ध्यान का अभ्यास करें।
इस कमरे को भगवान् का मन्दिर समझना चाहिए। आपको कमरे के भीतर पवित्रता सहित और आदरपूर्वक प्रवेश करना चाहिए। कमरे की चहारदीवारी के भीतर ईर्ष्या, वासना, लालच तथा क्रोध के विचारों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार की सांसारिक बातें नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी शब्द जो बोला गया हो, कोई भी विचार जो सोचा गया हो, कोई भी कार्य जो किया गया हो, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। वे जहाँ पर किये जाते हैं, उस कमरे के आकाश की सूक्ष्म लहर से टकरा कर परावर्तित होते हैं, इसलिए वे मन पर अनिवार्य रूप से प्रभाव डालते हैं।
जब आप भगवान् के नाम का उच्चारण करते हैं, तो वे कमरे के आकाश के शक्तिशाली स्पन्दन में स्थिर हो जाते हैं। छह माह के भीतर आपको कमरे के वातावरण में शान्ति और पवित्रता का अनुभव होगा। जब भी आपका मन सांसारिक प्रभावों से बहुत अधिक व्यथित हो, तब आप कमरे में बैठ जायें और आधे घण्टे तक भगवान् के नाम का जप करें। तब आप तत्काल मन के भीतर सम्पूर्णतया परिवर्तन देखेंगे। अभ्यास करें और शान्ति प्रदान करने वाले आध्यात्मिक प्रभावों का स्वयं अनुभव करें। आप मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, ऊटी स्वयं अपने ही घर में पायेंगे। आपको परिवर्तन हेतु किसी पर्वतीय स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
साधना अथवा योगाभ्यास के समान कुछ और चीज़ नहीं है।
६. ध्यान हेतु स्थान
"व्यक्ति को अपना ध्यान एकाग्रतापूर्वक एक ऐसे समतल स्थान पर करना चाहिए जो कंकर पत्थरों, अग्नि, वायु, धूल, शीत और कोलाहल से मुक्त हो, जहाँ का दृश्य नेत्रों को मनोहर, सुखकर हो, जहाँ कुटिया, गुफाएँ और उत्तम जल स्थान हो तथा जो उत्तम ध्यान में सहायता करे।” (श्वेताश्वतरोपनिषद् : ११-१०)
जब आप ध्यान में प्रगति करेंगे, तो संसार आपको रास नहीं आयेगा। यहाँ आपको बाधा डालने वाले अनेक कारण हैं। यहाँ का वातावरण उत्थानकारी नहीं है। आपके मित्र आपके सबसे बुरे शत्रु हैं। वे व्यर्थ की बातों में आपका सारा समय व्यर्थ गँवा देंगे। मित्रता करने पर ऐसा होना अनिवार्य है। आप परेशान हो जायेंगे। आप चिन्ता में पड़ जायेंगे। तब आप ऐसे वातावरण से बाहर निकलना चाहेंगे। समय, धन तथा भटकने को बचाने के लिए मैं आपको ध्यान हेतु कुछ स्थान बताना चाहता हूँ। आप इनमें से कोई एक स्थान चुन लें। यह स्थान समशीतोष्ण मौसम वाला होना चाहिए तथा यह ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा ऋतु में अनुकूल होना चाहिए। आपको दृढ़ निश्चय के लिए एक स्थान पर दृढ़तापूर्वक तीन वर्षों तक रहना होगा। चूँकि प्रत्येक स्थान के कुछ लाभ और कुछ हानियाँ हैं, इसलिए आपको ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ लाभ अधिक हों और हानियाँ कम। इस जगत् में प्रत्येक वस्तु एक-दूसरे से सम्बन्धित है। यहाँ तक कि यदि आप एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक चले जायेंगे, तो भी आपको एक आदर्श स्थान भी कठिनाई से प्राप्त हो सकेगा, जिससे आप सभी दृष्टिकोणों से सन्तुष्ट हो सकेंगे। आपको जप, ध्यान और प्रार्थना से अपना स्वयं का आध्यात्मिक वातावरण तैयार करना होगा। एक आदर्श स्थान प्राप्त करना असम्भव है। आपको थोड़ी असुविधा होने पर उस स्थान से हटना नहीं चाहिए। आपको वहीं रहना चाहिए। जल्दी-जल्दी स्थान बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। एक स्थान से दूसरे की तुलना न करें। अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करें। जब आप शिमला में होंगे, तो आपको मसूरी बड़ा ही आकर्षक अनुभव होगा और जब आप मसूरी में होंगे, तो शिमला बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होगा। मन तथा इन्द्रियों पर तनिक भी विश्वास न करें, उनकी चालें बहुत हो गयीं। इन्द्रियों के भ्रमित करने तथा प्रलोभनों से बचें।
सर्वप्रथम मैं ऋषिकेश और मुनिकीरेती का सुझाव दूँगा। ये ध्यान हेतु अद्भुत स्थान हैं। इनको प्रशंसनीय ढंग से स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ का आकर्षण तथा आध्यात्मिक प्रभाव अद्भुत है। आप यहाँ अपनी कुटिया बना सकते हैं। उत्तरकाशी, गरुड़चट्टी, ब्रह्मपुरी और नीलकण्ठ (ऋषिकेश के पास) अन्य अच्छे स्थान हैं। अल्मोड़ा और नैनीताल भी अच्छे हैं। गंगा, नर्मदा तथा यमुना के किनारे का प्रत्येक गाँव सुन्दर है। कुल्लु घाटी तथा चम्बा घाटी भी अनुकूल है। यदि आप गुफा में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश से १४ मील दूर वसिष्ठ गुहा चले जाइए। यह एक सुन्दर गुफा है। यहाँ पर स्वामी रामतीर्थ ने कुछ समय तक निवास किया था। यहाँ आस-पास के गाँवों में दूध भी उपलब्ध हो जाता है। ऋषिकेश के पास ब्रह्मपुरी में राम गुहा एक अन्य अच्छा सुन्दर स्थान है। आपको काली कमली वाला क्षेत्र से १५ दिनों के लिए राशन प्राप्त हो जायेगा। हिमालय में टिहरी के पास बामरुगी गुहा एक अच्छी गुफा है। आपको टिहरी के पास धारणा के लिए अनेक उत्तम स्थान मिलेंगे। मुरलीधर ने एक सुन्दर बगीचे सहित एक पक्की कुटिया बनायी है। आप यहाँ पर भी निवास कर सकते हैं। माउंट आबू भी एक सुन्दर और शीतल स्थान है।
ध्यान हेतु शीतल स्थान की आवश्यकता होती है। गर्म स्थान में मस्तिष्क अत्यन्त शीघ्र थक जाता है। शीतल स्थान में आप २४ घण्टे तक भी ध्यान कर सकते हैं। आपको थकावट का अनुभव नहीं होगा। अलवर और लिंबड़ी के महाराजा ने पढ़े-लिखे साधुओं के लिए माउंट आबू में अच्छी गुफाओं का निर्माण किया है तथा भोजन आदि अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की है। लक्ष्मणझूला एक अन्य उत्तम स्थान है। यहाँ नयी कुटिया के निर्माण हेतु भी बहुत स्थान है। कानपुर के पास ब्रह्मावर्त भी अनुकूल स्थान है। मथुरा के आगे सात मील दूर यमुना नदी के किनारे अनेक अच्छे स्थान है। उत्तरकाशी में आध्यात्मिक तरंगें अच्छी हैं। आप लक्षेश्वर नामक शान्त स्थान पर ठहर सकते हैं।
ध्यान हेतु महत्त्वपूर्ण स्थान
१. ऋषिकेश २. हरिद्वार
३. उत्तरकाशी ४. कनखल
५. बद्रीनारायण ६. देवप्रयाग
७. गंगोत्री ८. अयोध्या
९. माउंट आबू १०. नासिक
११. वाराणसी १२. वृन्दावन
१३. श्रीनगर १४. अल्मोड़ा
१५. नैनीताल १६. बेंगलुरु
१७. पुरी १८. द्वारका
१९. पण्ढरपुर २०. तिरुवोत्तियुर
२१. आलन्दी (पूना के पास) २२. तिरुवेनगोई पहाड़ियाँ (मुसिरी, दक्षिण भारत)
२३. तिरुपति की पहाड़ियाँ २४. पापनासम् (तिरुनेवेली जिला)
(इन स्थानों में से कोई शान्त स्थान चुन लें।)
गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और ताम्रपर्णी के किनारे का कोई भी गाँव आपको ध्यान हेतु अनुकूल होगा। आप कोई भी वह स्थान चुन सकते हैं, जो समशीतोष्ण वातावरण वाला हो।
सभी स्थानों में से और सारे संसार में से ऋषिकेश सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ पर आध्यात्मिक स्पन्दन आत्मोत्थानकारी हैं। दृश्यावली अत्यन्त आकर्षक है। यह एक सुन्दर स्थान है।
मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, ऊटी, कोडाईकेनाल तथा सभी पहाड़ी क्षेत्र शीतल स्थान हैं। वहाँ पर सुन्दर सुन्दर दृश्यावलियाँ हैं, लेकिन ये राजसिक क्षेत्र हैं। वहाँ पर कोई आध्यात्मिक उत्थानकारी स्पन्दन नहीं हैं। लोग वहाँ पर आनन्द लेने के लिए तथा वातावरण को दूषित करने के लिए जाते हैं। इसलिए वे ध्यान हेतु उपयुक्त नहीं हैं।
प्रारम्भ में इन स्थानों पर आपको ये कुछ सुविधाएँ अवश्य होनी चाहिए जैसे पुस्तकालय, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन। वहाँ पर आपको दूध और फल उपलब्ध होने चाहिए, अन्यथा एक ही स्थान पर लम्बे समय तक साधना करना कठिन हो जायेगा। जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे, जब आप देह-चेतना से ऊपर उठ जायेंगे, तो आप कहीं भी निवास कर सकते हैं।
एकान्त और निरन्तर ध्यान—ये दोनों आत्म-साक्षात्कार हेतु महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। गंगा अथवा नर्मदा, हिमालय का दृश्य, प्यारे फूलों के बगीचे, पवित्र मन्दिर—ये सभी वे स्थान हैं, जो ध्यान-धारणा में मन का उत्थान करते हैं, इनका लाभ लें।
एक शान्त स्थान, आध्यात्मिक स्पन्दन जो उत्तरकाशी, ऋषिकेश, बद्रीनारायण में हैं, एक अच्छा स्थान, सम वातावरण - ये स्थितियाँ मन की एकाग्रता हेतु अनिवार्य रूप से पूर्वापेक्षाएँ हैं।
७. ध्यान हेतु गुफा का जीवन
गुफा का जीवन ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने गुफाओं में रह कर कठोर तपस्या की थी। गुफाओं में तापमान एक जैसा रहता है। गुफाएँ ठण्ढी रहती हैं। जलाने वाली ग्रीष्म ऋतु की गर्मी गुफा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती।
किसी प्रकार की बाहरी आवाजें भी गुफा के भीतर नहीं सुनायी देतीं। | गुफा के भीतर आपका ध्यान सुन्दर और अबाधित होगा। गुफा के भीतर शान्ति भी रहती है। गुफा के भीतर के आध्यात्मिक स्पन्दन आत्मोत्थानकारी हैं। यहाँ लौकिक वातावरण भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आधुनिक सभ्यता प्रवेश नहीं कर सकती है। ये गुफा के जीवन के लाभ हैं।
हिमालय में वसिष्ठ गुफा अत्यन्त सुन्दर है। यह ऋषिकेश से १४ मील दूर है। यहाँ पर महर्षि वसिष्ठ ने तपस्या की थी। इस कारण इसका नाम वसिष्ठ गुफा है। यहाँ पर आपको पास के गाँवों से दूध प्राप्त हो सकता है। टिहरी हिमालय के पास बामरुघ गुफा एक अन्य अच्छी गुफा है। ऋषिकेश से ६ कि. मी. दूर नीलकण्ठ पहाड़ियों के पास भी गुफाएँ हैं।
जिनकी आधुनिक शिक्षा तथा दुर्बल शरीर है तथा जो भीरु हैं, उनके लिए गुफा में जीवन बिताना सम्भव नहीं है। यह उन साधकों के लिए है, जो मजबूत शरीर के स्वामी हैं, जो निर्भय हैं, जिनमें अत्यधिक सहन-शक्ति है, जिनके पास कुछ सिद्धियाँ हैं, वे यहाँ निवास कर सकते हैं। जिनको हिमालय की जड़ी-बूटियों का दिव्य अच्छा ज्ञान है, जिन्होंने कायाकल्प के द्वारा अपने शरीर को दृढ़ बना लिया है, जिन्होंने नीमकल्प अथवा शुद्ध कुचला के द्वारा जहरीले प्राणियों के काटने से स्वयं को प्रतिरोधी बना लिया है, जिनके पास मन्त्र-सिद्धि है, जिनका जंगली पशुओं के ऊपर नियन्त्रण है, जो सर्दी-गर्मी और भूख-प्यास को सहन कर सकते हैं, जिनको इस जगत्, इन्द्रिय-विषयों, किसी भी प्रकार के कार्य के प्रति कोई आकर्षण न शेष रहा हो, जो लम्बे समय तक ध्यान कर सकते हों, जिनको आन्तरिक वैराग्य हो, ऐसे सभी लोग गुफा में निवास कर सकते हैं।
कुछ युवा शुष्क साधक जिनका शरीर कमजोर है तथा दुर्बल स्वास्थ्य है, जिनमें कुछ धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से तथा जीवन में किसी दुर्भाग्य अथवा कुछ कठिनाइयों के कारण विवेक और वैराग्य की एक किरण जागी है, वे बिना किसी पूर्व-तैयारी अथवा शारीरिक और मानसिक संयम के हिमालय की गुफाओं की ओर दौड़ पड़ते हैं। जिस प्रकार थर्मामीटर का पारा तेज बुखार में १०६ डिग्री चढ़ जाता है, इसी प्रकार यौवन का जोश सिर के शीर्ष में ११२ डिग्री चढ़ जाता है। यह अत्यन्त शीघ्रता से ठण्ढा हो जाता है। उन्हें वहाँ रहने में कठिनाई का अनुभव होता है और कुछ ही दिनों में वे वह स्थान छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को गुफा का जीवन अनुकूल नहीं होता। उनको वायु का सही आवागमन न होने के कारण किसी प्रकार के त्वचा रोग अथवा पीत रुधिरता रोग हो जाता है।
किसी ऐसे स्थान में जहाँ वायु का अच्छा आवागमन है अथवा किसी भी एकान्त स्थान में यहाँ तक कि आपकी जमीन अथवा गाँव में भूमि के नीचे, दो दीवारों के बीच खाली स्थान में जिसमें ठण्ढी हवा तथा गर्म हवा हेतु पाइप हों (ये गुफा को ठण्डा रखेंगे) ऐसे किसी स्थान पर कृत्रिम गुफा जैसे कैवल्य गुहा अथवा आनन्द कुटीर निर्मित की जा सकती हैं। सभी सच्चे साधक जो संसार में रहते हैं, उन्हें अपने लिए ऐसी एक गुफा बना लेनी चाहिए। उन्हें अत्यधिक लाभ होगा।
गुफा के जीवन की एक और हानि है। जो लम्बे समय तक गुफा में निवास करते हैं, वे तामसिक हो जाते हैं। वे कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। वे लोगों के साथ घुल-मिल नहीं पाते। वे लोगों की भीड़ से बहुत घबराते हैं। यदि उन्हें कुछ लोगों के साथ रहना पड़ जाये, तो उनका सिर दर्द करने लगता है। यदि उन्हें थोड़ा भी शोर सुनायी देता है, तो उनका मन शीघ्र ही विचलित हो जाता है। यह सन्तुलित जीवन नहीं है। यह एकपक्षीय विकास है। जो गुफा में निवास करता है, उसे यदि वह एक व्यस्त शहर में जाये, तो भी अपना सन्तुलन बनाये रखना चाहिए। यही आध्यात्मिक विकास की पहचान है।
वास्तविक एकान्त, सुखद, अद्भुत गुहा आपके हृदय में है। यह उपनिषदों की हृदय-गुहा है, जहाँ प्राचीन काल में दत्तात्रेय, शंकर तथा याज्ञवल्क्य निवास करते थे। आज भी आधुनिक सन्त और ऋषि अपने बाहर की ओर भागने वाली इन्द्रियों और मन को भीतर खींच कर यहीं निवास करते हैं। वे यहाँ अमरता के मधु का पान करते हैं और सदा आनन्दमय रहते हैं।
आप सभी हृदय की इस रहस्यमय तथा अद्भुत गुफा में अपनी अन्तरात्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा, लक्ष्य तथा सभी के आत्मा के आश्रय के साथ अकेले लीन रहें।
८. ध्यान हेतु तैयारी
सिर, गर्दन तथा पीठ को एक सीधी रेखा में रखें। गीता के छठवें अध्याय के ११वें तथा १३वें श्लोक का पाठ करें, जहाँ आसन का वर्णन किया गया है। एक कम्बल को चारवर्ती करके बिछा लें और इसके ऊपर सफेद कपड़े का टुकड़ा बिछा लें। इस कार्य को अत्यन्त सुन्दरता से करें। यदि आपको एक अच्छा व्याघ्र चर्म अथवा हिरण की छाल मिल जाये, तो अत्युत्तम है। व्याघ्र चर्म के अपने ही लाभ हैं। यह शरीर में शीघ्र ही ऊर्जा प्रवाहित करता है और शरीर से ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता। यह चुम्बकत्व से परिपूर्ण है।
पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जायें। आध्यात्मिक नवाभ्यासी को इस नियम का पालन करना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुँह करने से वह हिमालय के ऋषियों के सम्पर्क में होगा और वह उनके प्रवाह से रहस्यमय ढंग से लाभान्वित होगा।
९. ध्यान कैसे करें
ध्यान की आदत तथा एकान्त आध्यात्मिक पथ में आपकी महान् धरोहर हैं। ध्यान आपको आध्यात्मिक शक्ति, शान्ति, नया बल तथा जीवनी-शक्ति प्रदान करता है। यदि ध्यान करने वाला अत्यन्त शीघ्र उत्तेजित हो जाता है, तो यह इस बात को दर्शाता है कि उसका ध्यान भली प्रकार और निर्बाध रूप से नहीं लग रहा है। उसकी साधना और ध्यान में कुछ गलती अवश्य है।
आपको शान्त मन के साथ ध्यान करना चाहिए। मात्र तभी आप शीघ्र समाधि में प्रविष्ट हो सकेंगे। यदि आप इन्द्रियों को नियन्त्रित कर लें और निष्काम हो जायें, तो आपका मन शान्त होगा। मुक्ति की प्रबल लालसा और ईश्वर के विचार शीघ्र ही आपको निष्काम बना देंगे। जिसका मन शान्त है, वह सम्राटों का सम्राट्, शाहों का शाह है। जिसका मन शान्त है, उसकी स्थिति अवर्णनीय है।
धारणा और ध्यान में आपको मन को अनेक प्रकार से प्रशिक्षित करना होगा। मात्र तभी आपका स्थूल मन सूक्ष्म बनेगा।
जो भी आप एकान्त में ध्यान करेंगे, वह आपके नित्य के जीवन में परिलक्षित होना चाहिए। आपके कार्यों में सन्तुलन तथा सामंजस्य होना चाहिए। आपको सदैव शान्तिपूर्ण होना चाहिए। मात्र तभी आप ध्यान के परिणामों का वास्तव में साक्षात्कार कर सकेंगे।
ध्यान की प्रक्रिया
ऊपर के अंगों (धड़, गर्दन तथा सिर) को सीधे और शरीर के बराबर रखते हुए मन को इन्द्रियों सहित हृदय में लीन कर दें। ज्ञानी ब्रह्म (ॐ) की पतवार से संसार की सभी भयंकर यन्त्रणाओं से पार हो जाता है।
इन्द्रियों को नीचे रख कर, अपनी कामनाओं को वशीभूत करके तथा नासारन्ध्रों से ज्ञानी को अपने मन को उसी प्रकार नियन्त्रित करना चाहिए, जिस प्रकार एक रथ का सारथी बिगड़े हुए घोड़ों के द्वारा खींच कर ले जाये जा रहे रथ पर नियन्त्रण करता है।
योगी के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित शरीर में धारणा के निम्न वर्णित लक्षण प्रकट होते हैं। उसके लिए कोई रोग अथवा आयु अथवा कष्ट नहीं होता, जिसने अपने शरीर को धारणा की अग्नि से जला डाला है।
जब शरीर हल्का और निरोग होता है, मन कामनाओं से रहित होता है, जब रंग तेजस्वी होता है, वाणी मधुर होती है तथा उसके शरीर से सुगन्ध आती है। जब मल-मूत्र अत्यन्त कम हो जाते हैं, तो कहते हैं कि प्रथम श्रेणी की धारणा प्राप्त हो गयी है।
सामान्य निर्देश
जिस प्रकार आप नमक अथवा शक्कर को जल से सन्तृप्त करते हैं, उसी प्रकार आपको मन को ईश्वर के विचारों के साथ, दैवी वैभव, दैवी उपस्थिति के साथ, श्रेष्ठ आत्मा को जाग्रत करने वाले आध्यात्मिक विचारों के साथ सन्तृप्त करना चाहिए। मात्र तभी आप सदैव दैवी चेतना में स्थित हो सकेंगे।
यदि आप कठोर ध्यानाभ्यास करना तथा शीघ्र समाधि प्राप्त करना अथवा आत्म-साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आपके लिए पाँच चीजें अनिवार्य हैं—मौन, हल्का आहार अथवा दूध और फलों का आहार, आकर्षक दृश्यावली सहित एकान्त, एक गुरु के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क एवं एक शीतल स्थान।
आप गहन ध्यान में मात्र तभी प्रवेश कर सकते हैं, जब आप नैतिक जीवन व्यतीत करें। इसके पश्चात् आपको अपने मन में विवेक और अन्य चरणों को निर्मित करना होगा। आप धारणा में मन का अर्जन कर सकते हैं और अन्त में स्वयं को ध्यान हेतु समर्पित कर सकते हैं। जितना अधिक आप नैतिक जीवन बितायेंगे, जितना अधिक आप ध्यान करेंगे, उतना ही अधिक आपको निर्विकल्प समाधि (जो कि आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगी तथा आपको अनन्त आनन्द और अमरता प्रदान करेगी) में प्रवेश करना सरल होगा। भगवान् श्री कृष्ण अपने हाथों में वंशी ले कर क्या शिक्षा देते हैं? वंशी का प्रतीकात्मक दर्शन क्या है? वंशी ॐ का प्रतीक है। वे कहते है- " अपने अहंकार को रिक्त कर दो। मैं तुम्हारी शरीर रूपी वंशी को बजाऊंगा। तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा से एक हो जाये। ॐ में शरण लो। तुम मुझमें प्रविष्ट हो जाओगे। आत्मा को झंकृत करने वाले आत्मा के आन्तरिक संगीत को सुनो और अनन्त शान्ति में विश्राम करो। "
हल्के आहार सहित धारणा तथा ध्यान के अभ्यास के द्वारा समाधि सम्भव है। दो या तीन घण्टे ध्यान करें। यदि आप थक गये हैं, तो आधे घण्टे विश्राम कर लें। एक कप दूध लें, तत्पश्चात् पुनः ध्यान हेतु बैठ जायें। ध्यान की क्रिया विधि को बार-बार दोहरायें। आप सन्ध्या के समय बरामदे में टहल सकते हैं। मन में यहाँ तक कि कुछ मिनट के लिए भी सांसारिक विचारों को न आने दें।
जिस प्रकार एक विद्यार्थी गणित अथवा भूगोल विषय अरुचिकर लगने पर भी परीक्षा में पास होने के बाद जो लाभ प्राप्त होते हैं, उनकी कल्पना करके उनके प्रति रुचि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आपको ध्यान के निरन्तर अभ्यास के द्वारा जो अगणित लाभ जैसे अमरता, परम शान्ति तथा अनन्त आनन्द प्राप्त होंगे, उनका विचार करके ध्यान में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए।
जब आपको काम के प्रति अरुचि तथा एकमात्र ध्यान की कामना होगी, तो आप दूध और फल मात्र पर आधारित पूर्ण संन्यास का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपकी अच्छी आध्यात्मिक प्रगति होगी। जब ध्यान की इच्छा समाप्त हो जाये, पुनः काम करने लगे। इस प्रकार शनैः-शनैः अभ्यास के द्वारा मन को मोड़ा जा सकता है।
एक लोहे का टुकड़ा जलती हुई भट्ठी में रखिए। यह अग्नि की भाँति लाल हो जायेगा। इसे हटा लें। यह अपना लाल रंग खो देगा। यदि आप इसे सदा लाल रखना चाहते हैं, तो आपको इसे सदा आग के ऊपर रखना होगा। इसी प्रकार यदि आप मन को ब्रह्मज्ञान से सदा आवेशित रखना चाहते हैं, तो आपको मन को निरन्तर ध्यान के द्वारा सदा ब्रह्माग्नि के सम्पर्क में रखना होगा। आपको ब्रह्म-चेतना के तैलधारावत् प्रवाह को बनाये रखना होगा। तब आपको सहज अवस्था प्राप्त होगी।
यदि आप आधा घण्टे ध्यान करते हैं, तो आप इसके बल से स्वयं को जीवन-संघर्ष में एक सप्ताह तक शान्ति तथा आध्यात्मिकता के साथ लगाये रखने में सक्षम होंगे। चूँकि आपको नित्य जीवन में विशेष प्रकार की प्रकृति वाले विभिन्न मनों के साथ चलना पड़ता है, इसलिए ध्यान से शान्ति और शक्ति प्राप्त करें। तब आपको कोई परेशानी और चिन्ता नहीं होगी।
जब आप ध्यान में नवाभ्यासी हों, तो ध्यान में बैठने के तत्काल बाद दस मिनट तक कुछ श्रेष्ठ श्लोकों का पाठ करें। यह मन का उत्थान करेगा। मन को सांसारिक विषयों से सरलता से वापस खींचा जा सकेगा। तत्पश्चात् इस प्रकार के विचार को भी रोक दें और मन को बार-बार तथा प्रयत्नपूर्वक एक ही विचार पर लगायें। तब निष्ठा प्रकट होगी।
चित्र
जब आप ध्यान प्रारम्भ करें, उसके पहले आपको अपने सामने भगवान् अथवा ब्रह्म का (स्थूल अथवा निर्गुण) मानसिक चित्र रखना चाहिए। जब आप भगवान् श्री कृष्ण का स्थूल चित्र खुली आँखों से देखेंगे और ध्यान करेंगे, तो यह ध्यान का स्थूल रूप है। जब आप अपनी आँखें बन्द करके भगवान् श्री कृष्ण का चित्र देखेंगे, तो यह भी स्थूल ध्यान है; लेकिन यह अधिक निर्गुण है। जब आप अनन्त निर्गुण प्रकाश का ध्यान करते हैं, तो यह और अधिक निर्गुण है। पूर्व वाले दोनों ध्यान के सगुण प्रकार से सम्बद्ध हैं। निर्गुण ध्यान में भी प्रारम्भ में मन को स्थिर करने के लिए एक निर्गुण रूप है। बाद में यह रूप नष्ट हो जाता है और ध्यान तथा ध्याता एक हो जाते हैं। ध्यान मन से आगे बढ़ता है।
व्यावहारिक निर्देश
ध्यान के समय देखें कि आप कितने समय तक सभी सांसारिक विचारों को बन्द कर सकते हैं। मन को बड़ी ही सावधानीपूर्वक देखें। यदि यह समय बीस मिनट है, तो इसे तीस मिनट अथवा अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करें। मन को बार-बार दैवी विचारों से भरें। जब मन ध्यान में स्थिर हो जाता है, तो नेत्र गोलक भी स्थिर हो जाते हैं। एक योगी जिसका मन शान्त है, उसके नेत्र स्थिर होते हैं। पलकें झपकनी नहीं चाहिए। आँखें लाल अथवा श्वेत होनी चाहिए।
सभी कार्य चाहे वे आन्तरिक अथवा बाह्य हों, वे मात्र तभी किये जा सकते हैं, जब मन अंगों के साथ संयुक्त होता है। विचार ही सच्चा कर्म है। यदि आपने स्थिर अभ्यास से मन पर नियन्त्रण कर लिया है, यदि आप आवेगों और चित्त-वृत्तियों को नियमित कर सकते हैं, तो आप मूर्खतापूर्ण और गलत कार्य नहीं कर सकते। ध्यान विभिन्न आवेगों और चित्त वृत्तियों पर नियन्त्रण में बहुत अधिक सहायता करता है।
विस्तृत आकाश पर धारणा और ध्यान करें। यह एक अन्य प्रकार का निर्गुण ध्यान है। ध्यान की इस विधि से मन सीमित रूपों के विचारों को बन्द कर देता है। यह धीरे-धीरे शान्ति के सागर में बदलने लगता है अर्थात् यह इसके विषय अर्थात् विभिन्न प्रकार के रूपों से रहित हो जाता है। यह सूक्ष्म और अति सूक्ष्म हो जाता है।
कुछ साधक खुली आँखों से ध्यान करना पसन्द करते हैं, जब कि कुछ बन्द आँखों से, जब कि कुछ अन्य अधखुले नेत्रों से।
यदि आप खुली आँखों से ध्यान करेंगे, तो धूल आदि के कण आपकी आँखों में प्रविष्ट हो जायेंगे। कुछ विद्यार्थी खुली आँखों से धारणा करना पसन्द करते हैं, जब कि कुछ बन्द आँखों से। जो बन्द आँखों से ध्यान करते हैं, उन्हें थोड़ी ही देर में नींद आने लगती है। यदि आँखें खुली रहती हैं, तो प्रारम्भिक अभ्यासियों का मन विषयों पर घूमता रहता है। अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग कीजिए और उस विधि को अपनाइए जो आपको अनुकूल आये। किसी भी परिस्थिति में जो भी अन्य बाधाएँ आयें, उन पर विजय प्राप्त कीजिए।
आपको ध्यान के अभ्यास में नियमित रहना चाहिए। ध्यान में नियमितता महान् आवश्यक है । अभ्यासी यदि नियमित रहे, तो उसकी प्रगति अत्यन्त शीघ्र होती है एवं उसे महान् सफलता प्राप्त होती है। यहाँ तक कि यदि आपको कोई वांछित परिणाम न भी प्राप्त हों, तो भी आपको लगनशीलता, धैर्य तथा अध्यवसाय के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। कुछ समय बाद आपको महान् सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। किसी भी परिस्थिति में एक दिन के लिए भी अभ्यास न रोकें। मन को बार-बार सात्त्विक दैवी विचारों से परिपूर्ण करें। अब नयी लीकों का निर्माण हो जायेगा। जिस प्रकार एक ग्रामोफोन की सुई प्लेट में एक छोटी लीक का निर्माण करती है, उसी प्रकार सात्त्विक विचार मन एवं मस्तिष्क में नयी स्वस्थ लीकों को काटता है। नवीन संस्कारों का निर्माण होता है।
प्राण मन के लिए बाहरी आवरण है। सूक्ष्म प्राण के स्पन्दन विचारों के निर्माण को जन्म देते हैं। प्राणायाम के द्वारा आप मन को अधिक सूक्ष्म बना कर अपने ध्यान में वृद्धि कर सकते हैं।
यदि आप नीबू के रस अथवा इमली के रस को एक सोने के प्याले में रखें, तो वह खराब नहीं होता; लेकिन यदि आप इसे ताँबे अथवा पीतल के बर्तन में रख दें, तो यह उसी समय खराब हो कर विषैला हो जायेगा। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति जो निरन्तर ध्यान का अभ्यास करता है, उसके शुद्ध मन में यदि थोड़ी विषय-वृत्ति भी होगी, तो वह उस व्यक्ति को प्रदूषित नहीं करेगी और विकार (विषय-विचारों) को प्रेरित नहीं करेगी। यदि अशुद्ध मन वाले व्यक्तियों में विषय-विचार होंगे, तो जब भी वे विषय-वस्तुओं के सम्पर्क में आयेंगे, तब वे उनमें उत्तेजना उत्पन्न करेंगे।
शारीरिक स्वास्थ्य
आसन शरीर को स्थिर बनाते हैं। बन्ध और मुद्राएँ शरीर को दृढ़ बनाते हैं। प्राणायाम शरीर को हल्का बनाता है। नाड़ी शुद्धि मन की साम्यावस्था को प्रभावित करती है। इन योग्यताओं का अर्जन करके आपको मन को ब्रह्म पर केन्द्रित करना चाहिए। तभी ध्यान स्थिरतापूर्वक आनन्द के साथ हो सकेगा।
प्रातःकाल ४ बजे पाँच मिनट शीर्षासन करें। इसके बाद पाँच मिनट विश्राम करें। तत्पश्चात् बैठ कर ध्यान करें। आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा।
ध्यान के पूर्व २० हल्के कुम्भक करें, तत्पश्चात् ध्यान हेतु बैठ जायें। प्राणायाम तन्द्रा और निद्रा को दूर कर देगा और मन को स्थिर बनायेगा।
एक सप्ताह तक मात्र फल और दूध पर रहें। आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। यह आहार आपको हल्का और सात्त्विक बनायेगा। रात्रि के समय ध्यान रखें, मात्र आधा सेर दूध ही लें। आपका अच्छा ध्यान लगेगा। आप नींद पर शीघ्र विजय प्राप्त कर सकेंगे। रात्रि के समय भारी भोजन से आलस्य शीघ्र आता है।
ध्यान के आसन
जो ४-५ घण्टे लगातार ध्यान करते हैं, उन्हें प्रारम्भ में पद्मासन तथा वज्रासन अथवा सिद्धासन और वज्रासन में बैठना चाहिए।
कभी-कभी पैरों अथवा जाँघों के भागों में रक्त एकत्रित हो जाता है और थोड़ी परेशानी देता है। दो घण्टे के बाद पद्मासन अथवा सिद्धासन से वज्रासन में बैठ जायें अथवा पैरों को पूरे सीधे फैला दें। एक दीवार अथवा तकिये से टिक कर बैठें। मेरुदण्ड सीधा रखें। यह अत्यन्त आरामदायक आसन है। दो कुर्सियों को आपस में जोड़ लें, एक कुर्सी पर बैठ जायें और दूसरी पर पैर फैला लें। यह भी एक अन्य युक्ति है।
यह प्रारम्भिक अभ्यासियों के लिए एक प्रकार का ध्यान है। एक एकान्त कमरे में पद्मासन में बैठें। अपनी आँखें बन्द कर लें। सूर्य के तेज, चन्द्रमा के वैभव, तारों की द्युति और आकाश के सौन्दर्य पर ध्यान करें।
प्रारम्भिक योग्यताएँ
प्रारम्भ में धारणा में मन को विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण दें। कानों को बन्द करके हृदय की अनाहत ध्वनियों पर धारणा करें। 'सोऽहं' का जप करते हुए श्वास पर धारणा करें। किसी भी स्थूल प्रतीक पर धारणा करें। सूर्य के सर्वव्यापक प्रकाश पर धारणा करें। नीले आकाश पर धारणा करें। शरीर के विभिन्न चक्रों पर धारणा करें। सत्य, ज्ञान, अनन्त, एक, नित्य आदि निर्गुण विचारों पर धारणा करें। अन्त में एक ही चीज पर दृढ़ हो जायें।
ध्यान में आँखों पर जोर न डालें। मस्तिष्क पर तनाव न दें। मन के साथ संघर्ष न करें। दिव्य विचारों को सरलतापूर्वक प्रवाहित होने दें। स्थिरतापूर्वक ध्यान के लक्ष्य के बारे में विचार करें। अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले विचारों को ऐच्छिक रूप से तथा हिंसात्मक रूप से भगाने का प्रयास न करें। श्रेष्ठ सात्त्विक विचार रखें।
यदि ध्यान में कोई तनाव हो, तो कुछ दिनों के लिए ध्यान के घण्टों को कुछ कम कर दें। मात्र हल्का ध्यान करें। जब आप सामान्य अवस्था में आ जायें, तो पुनः समय में वृद्धि करें। सम्पूर्ण साधना में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें। मैं हमेशा इसी बात पर जोर देता हूँ।
१०. कब और कहाँ ध्यान करें
ब्राह्ममुहूर्त में ध्यान का अभ्यास करें। यह ध्यान हेतु सर्वश्रेष्ठ समय है। सदैव दिन और रात के उस समय का चुनाव करें, जब आपका मन स्वच्छ हो और जब आप कम बाधित हो। आपको सोने जाने के पूर्व एक बार ध्यान हेतु बैठना चाहिए। मन इस समय बड़ा ही शान्त रहता है। आपका ध्यान रविवार को बड़ा ही अच्छा लगेगा; क्योंकि यह छुट्टी का दिन है और मन मुक्त रहता है। रविवार के दिन कठोर ध्यानाभ्यास कीजिए। जब आप मात्र फल और दूध पर रहेंगे अथवा उपवास करेंगे, तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। सदैव अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करें और ध्यान में अधिक लाभ प्राप्त करें।
रात्रि में ध्यान करें। दूसरी बार बैठक अनिवार्य है। रात में यदि आपके पास अधिक अवकाश नहीं है, तो कुछ मिनट अर्थात् मात्र १० या १५ मिनट ही बैठें। आपको रात के समय बुरे स्वप्न नहीं आयेंगे। निद्रा में भी दिव्य विचार रहेंगे। उस समय अच्छे संस्कार रहेंगे।
एक साधक जो कि शहर में एक एकान्त कमरे में ध्यान करता है, उसे वहाँ पर भी उतनी ही शान्ति प्राप्त हो सकती है जितनी कि एक जंगल में होगी। लेकिन उसे वहाँ पर ऋषिकेश, उत्तरकाशी अथवा गंगोत्री के समान आध्यात्मिक स्पन्दन नहीं प्राप्त हो सकते। मन के उत्थान तथा मन की एकाग्रता उत्पन्न करने में स्पन्दन एक जीवन्त भूमिका अदा करते हैं। इन पवित्र स्थानों में ऋषियों के स्पन्दन फैले हुए हैं और साधकों को उनसे बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। इन पवित्र स्थानों में बिना किसी संघर्ष अथवा प्रयत्न के स्वयं ही वैराग्य, सात्त्विक भाव आ जाता है। कुछ स्त्रियाँ ऋषिकेश स्टेशन पर नीचे उतर जाती हैं। जिस क्षण वे हिमालय को देखती हैं, वे कहती हैं- "बेटा कौन है? पिता कौन है? प्रत्येक चीज़ माया है। हर चीज़ झूठी है।" यहाँ मन पर ऐसा शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। मात्र योगी और सन्त ही हैं, जो तत्काल ध्यान के स्थान के स्पन्दनों को जान सकते हैं।
आपको जीवन के अनेक रहस्यों को खोलने की चाबी दे दी गयी है। यह चाबी है ध्यान। प्रातःकाल ४ से ७ बजे के बीच नियमित रूप से ध्यान कीजिए और अनन्त आनन्द तथा अमरता को प्राप्त कीजिए।
गंगा और नर्मदा के किनारे, हिमालय का दृश्य, सुन्दर फूलों के बगीचे तथा पवित्र मन्दिर—ये वे स्थान हैं, जो धारणा और ध्यान में मन का उत्थान करते हैं। ऐसे स्थानों पर ध्यान कीजिए।
एकएकान्त स्थान जहाँ मौसम ठण्ढा हो और जहाँ आध्यात्मिक स्पन्दन हों, मन की धारणा हेतु उत्तम है।
प्रातःकाल के समय आपका मन स्वच्छ और शान्त होता है। उस समय आध्यात्मिक प्रभाव तथा अद्भुत शान्ति होती है। सभी सन्त तथा योगी इस समय ध्यान का अभ्यास करते हैं और सम्पूर्ण जगत् को अपने आध्यात्मिक स्पन्दन भेजते हैं। यदि आप इस समय अपनी प्रार्थना, जप और ध्यान प्रारम्भ करें, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। मन की ध्यानावस्था स्वयं ही आयेगी।
११. ध्यान की पूर्वापेक्षाएँ
जब मन निर्विषय (विषय-वस्तुओं तथा उनके उपभोग के विचार से मुक्त) बन जाये, तो यह ध्यान है।
भगवान् ने स्वयं को इस संसार में छिपाया है और आपकी हृदय गुहा में बैठ गये हैं। वे अदृश्य स्वामी हैं। आपको शुद्ध मन के साथ धारणा और ध्यान के द्वारा उनकी खोज करनी होगी। यह लुका-छिपी का यथार्थ खेल है।
ध्यान के लिए प्रत्येक वस्तु सात्त्विक होनी चाहिए। भोजन भी सात्त्विक होना चाहिए। पहना हुआ वस्त्र भी सात्त्विक होना चाहिए। संगत भी सात्त्विक होनी चाहिए। बातचीत भी सात्त्विक होनी चाहिए। स्वाध्याय भी सात्त्विक होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु सात्त्विक होनी चाहिए। तभी मात्र अच्छी प्रगति सम्भव है, विशेष रूप से नवाभ्यासियों के विषय में यह अनिवार्य है।
अनिवार्यताएँ
(१) उत्तरकाशी, ऋषिकेश, लक्ष्मणझूला, कनखल अथवा बद्रीनाथ जैसा शीतल स्थान ध्यान हेतु अनिवार्य
है, क्योंकि ध्यान के समय मस्तिष्क गर्म हो जाता है।
(२) साधना हेतु क्षमता।
(३) अच्छा, सात्त्विक, सारभूत, हल्का और पोषक आहार ।
(४) एक अच्छा आध्यात्मिक (अनुभवी) गुरु।
(५) अध्ययन हेतु उत्तम पुस्तकें।
(६) आपके भीतर ज्वलन्त वैराग्य, ज्वलन्त मुमुक्षुत्व तथा दृढ़ विवेक ।
(७) आपमें ब्रह्म-तत्त्व, ब्रह्म-वस्तु को समझने के लिए सूक्ष्म, तीव्र, शान्त तथा एकाग्र बुद्धि होनी
चाहिए। मात्र तभी साक्षात्कार सम्भव है। अनेक लोगों को आध्यात्मिक साधना के लिए उपर्युक्त
अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं प्राप्त होतीं। यही कारण है कि वे किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते।
ध्यान तभी सम्भव है, जब मन सत्त्व गुण से परिपूर्ण हो। पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। मन एवं भोजन के मध्य अन्तरंग सम्बन्ध है। भारी भोजन हानिकारक है। ११ बजे पूरा भोजन लीजिए और रात्रि के समय आधा सेर दूध लें। जो ध्यान करते हैं, उन साधकों के लिए रात्रि भोजन हल्का होना चाहिए।
प्रत्येक मनुष्य के भीतर अनेक योग्यताएँ एवं क्षमताएँ हैं। वह शक्ति एवं ज्ञान का कोष है। वह जैसे-जैसे विकास करता है, उसकी नयी शक्तियाँ और क्षमताएँ और योग्यताएँ अनावृत होती जाती हैं। अब वह अपने वातावरण को परिवर्तित कर सकता है और अन्यों को प्रभावित कर सकता है। वह अन्यों के मन को वशीभूत कर सकता है। वह आन्तरिक तथा बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह परम चेतनावस्था में प्रवेश कर सकता है।
एक अँधेरे कमरे में एक बर्तन रखा है, जिसमें एक जलता हुआ दीपक है। यदि वह बर्तन फूट जाता है, तो कमरे का अँधेरा विलीन हो जाता है और आप कमरे में सर्वत्र उजाला देखते हैं। इसी प्रकार यह शरीर रूपी बर्तन यदि आत्मा के ऊपर निरन्तर ध्यान करने से फूट • जाये अर्थात् यदि आप अविद्या और इसके प्रभाव - शरीर के साथ पहचान को नष्ट कर दें और शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जायें, तो आप आत्मा के परम प्रकाश को सर्वत्र देख सकते हैं।
आसन वास्तव में मानसिक हैं। मानसिक पद्मासन अथवा मानसिक सिद्धासन लगाने का प्रयास करें। यदि मन भटकता है, तो आपका शरीर अथवा आसन स्थिर नहीं होगा। जब मन स्थिर होगा अथवा ब्रह्म में दृढ़ होगा, तो शरीर की स्थिरता स्वयं ही आयेगी।
निरन्तर ईश्वर के बारे में विचार करें। मन को सदैव ईश्वर की ओर जाना चाहिए। मन को एक महीन रेशमी तन्तु से भगवान् शिव अथवा हरि के चरणों से बाँध दीजिए। मन के भीतर सांसारिक विचारों को प्रवेश न करने दें। मन को किसी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक सुख के बारे में विचार न करने दें। जब यह उपर्युक्त विचारों में लिप्त हो, तो इसकी अच्छी पिटाई करें। तब यह भगवान् की ओर मुड़ेगा। जिस प्रकार गंगा निरन्तर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार भगवान् के विचार निरन्तर बिना रुके प्रभु की ओर प्रवाहित होने चाहिए। जिस प्रकार घण्टियों की आवाज एक लय में कानों में पड़ती है, उसी प्रकार मन को भगवान् की ओर एक निरन्तर बहती धारा में आना चाहिए। निरन्तर साधना के द्वारा सात्त्विक मन से ईश्वर की ओर निरन्तर दैवी वृत्ति का प्रवाह होता रहना चाहिए।
किसी भी चीज पर किसी प्रकार विचार न करना सर्वोच्च समाधि प्राप्त करना है।
निदिध्यासन अथवा निरन्तर और श्रेष्ठ ध्यान में विचार करने की प्रक्रिया रुक जाती है। तब वहाँ मात्र एक ही विचार रहता है—'अहं ब्रह्मास्मि ।' जब यह विचार भी त्याग दिया जाता है, तो निर्विकल्प समाधि होती है।
मन रूपों के द्वारा निराकार को पकड़ना चाहता है। मन के शुद्धिकरण के बाद श्रवण (आध्यात्मिक प्रवचनों तथा पवित्र ग्रन्थों के श्रवण) एवं ब्रह्म-चिन्तन के द्वारा एक निराकार प्रतीक निर्मित होता है। बाद में गहन ध्यान में यह निराकार प्रतीक विलीन हो जाता है। जो शेष रह जाता है, वह है चिन्मात्र अथवा केवल अस्ति (शुद्ध अस्तित्व मात्र ) ।
मन की पूजा ब्रह्म की भाँति की जानी चाहिए। यह बौद्धिक पूजा है, यह उपासना-वाक्य है।
मन ब्रह्म अथवा प्रकट ईश्वर है। मन चलता-फिरता ईश्वर है।
ब्रह्म तक मन के साधन द्वारा पहुँचा जा सकता है। यह ही उचित है कि मन के ऊपर ब्रह्म की भाँति ध्यान किया जाये।
यदि कर्मयोग के साधक आत्मज्ञान के साथ व्यवहार करते हुए, अपने अन्तर में आनन्द प्राप्त करते हैं और तत्काल फल प्राप्ति की लालसा नहीं करते और नियमित रूप और धीरे-धीरे से ध्यान करते हैं, तब मन धीरे-धीरे परिपक्क होता है और अन्त में वे अनन्त आत्मा तक पहुँच जाते हैं।
जब आप एक पुस्तक को अत्यन्त ध्यान से रुचिपूर्वक पढ़ते हैं, तो आपका मन विचारों में लीन हो जाता है; उसी प्रकार ब्रह्म के निर्गुण ध्यान में मन एक ही विचार पर दृढ़ हो जाता है और वह है आत्मा का ध्यान ।
आपको ध्यान के लिए एक प्रशिक्षित उपकरण (मन) की आवश्यकता है। इसे शान्त, स्पष्ट, शुद्ध, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, स्थिर तथा एकाग्र होना चाहिए। ब्रह्म शुद्ध और सूक्ष्म है। इस कारण आपको ब्रह्म तक पहुँचने के लिए शुद्ध और सूक्ष्म मन की आवश्यकता है।
एक एकान्त स्थान में पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन में बैठ जाइए। स्वयं को सभी प्रकार की वासनाओं, आवेगों और आवेशों से मुक्त करें। इन्द्रियों को वश में करें। मन को विषयों से खींच लें। बाहरी अथवा सांसारिक विचारों को सहजता से भगायें। ॐ अथवा 'अहं ब्रह्मास्मि' का बार-बार मानसिक जप करके ब्रह्माकार-वृत्ति बनाये रखने का प्रयत्न करें। ॐ के मानसिक जप के साथ अनन्त का विचार, प्रकाश के सागर का विचार, सर्वज्ञान का विचार तथा सर्व आनन्द का विचार आता है। यदि मन भटकता है, तो साढ़े तीन मात्रा के दीर्घ प्रणव का उच्चारण ६ बार करें। यह विधि विक्षेप तथा अन्य बाधाओं को दूर करेगी।
मन कठोर परिश्रम के बाद थकान का अनुभव करता है। इसलिए यह आत्मा नहीं बन सकता। आत्मा अनन्त शक्ति का कोष है। मन आत्मा का उपकरण मात्र है। इसे उचित प्रकार से संयमित करना चाहिए। जिस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के व्यायामों के द्वारा अपने भौतिक शरीर का विकास करते हैं, उसी प्रकार आपको मानसिक प्रशिक्षण, मानसिक चरित्र अथवा मानसिक व्यायाम के द्वारा मन को प्रशिक्षित करना होगा।
जिस प्रकार नमक जल में घुल जाता है, उसी प्रकार सात्त्विक मन एकान्त में ध्यान के समय ब्रह्म में, इसके अधिष्ठान में विलीन हो जाता है।
ॐ धनुष है, मन तीर है तथा ब्रह्म वह लक्ष्य है जिसे वेधा जाना है। ब्रह्म उसके द्वारा वेधा जा सकता है, जिसके विचार केन्द्रित हैं। ऐसा होने पर यह मन ब्रह्म के साथ उसी प्रकार तन्मय हो जाता है, जैसे कि तीर लक्ष्य को वेधने के बाद उसके साथ एक हो जाता है।
ध्यानाभ्यास के लिए ब्राह्ममुहूर्त का समय (प्रातःकाल ४ से ६ बजे तक) निस्सन्देह सर्वश्रेष्ठ समय है। यह वह समय है, जब अच्छी नींद के पश्चात् मन एकदम तरोताजा रहता है। इस समय मन तुलनात्मक रूप से शान्त और शुद्ध रहता है। यह कोरे कागज के समान होता है। मात्र ऐसा मन ही वैसे आकार में ढाला जा सकता है जैसा आप चाहें। और इस समय वातावरण भी शुद्धता तथा अच्छाई से आवेशित रहता है।
यदि आप ध्यानयोग का अभ्यास करना चाहते हैं, यदि आप मन की धारणा के द्वारा भगवद्-साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सभी भौतिक गतिविधियाँ पूर्णतया बन्द कर देनी चाहिए। ५ या ६ वर्षों के लिए सभी मोह के बन्धन निर्दयतापूर्वक काट दिये जाने चाहिए। समाचार पत्र पढ़ना और मित्रों से पत्र-व्यवहार पूर्णतया बन्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये मन को विचलित करते हैं और संसार के विचार को दृढ़ करते हैं। ५ या ६ वर्षों के लिए एकान्त अनिवार्य है।
मन 'मैं' के कारण ही अस्तित्वमान है। 'मैं' मात्र मन का विचार है। मन और 'मैं' एक ही है। 'मैं' यदि नष्ट हो जाये, तो मन भी नष्ट हो जायेगा। यदि मन नष्ट हो जायेगा, तो 'मैं' भी नष्ट हो जायेगा। तत्त्वज्ञान के द्वारा मन को नष्ट कर दें। 'अहं ब्रह्मास्मि' की भावना के द्वारा, निरन्तर प्रबल निदिध्यासन के द्वारा 'मैं' का नाश कर दें। जब मन नष्ट हो जाता है, तो विचार रुक जाते हैं, नाम-रूप भी अस्तित्वमान नहीं रहते और आप लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं।
१२. ध्यान हेतु तीन बैठकें
प्रारम्भ में मात्र दो बार ध्यान हेतु बैठिए—एक बार प्रातः ४ से ५ बजे तक तथा दूसरी बार रात्रि में ६ से ८ बजे तक। ६ माह अथवा १ वर्ष के पश्चात् आप अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार तीन बार ध्यान हेतु बैठ सकते हैं। ऊपर की दोनों बैठकों के अलावा मध्याह्न में ४ से ५ बजे तक एक बार और आप धारणा का समय दो घण्टों तक बढ़ा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यह पसीने के कारण थोड़ा क्लेशकर तथा कठिन होता है। इस नुकसान की भरपाई शीत ऋतु में की जा सकती है। शीत ऋतु ध्यान हेतु बहुत अधिक अनुकूल है। ऋषिकेश और मुनिकीरेती ध्यान हेतु प्रशंसनीय ढंग से अनुकूल होंगे। ध्यान के नवाभ्यासियों के लिए शीत ऋतु तथा वसन्त ऋतु का आरम्भिक भाग श्रेष्ठ है। शीत ऋतु में मन बिलकुल भी नहीं थकता। आप थकान का थोड़ा भी अनुभव किये बिना २४ घण्टे ध्यान कर सकते हैं। यही कारण है कि साधु लोग शीत ऋतु में ध्यान हेतु ऋषिकेश का चुनाव करते हैं। ध्यान के समय में सावधानीपूर्वक शनैः-शनैः वृद्धि करनी चाहिए। ध्यान आवेश में आ कर प्रारम्भ नहीं करना चाहिए। इसे नियमित रूप से स्थिरतापूर्वक करना चाहिए। सम्पूर्ण साधना की अवधि में आपको अपने सामान्य ज्ञान एवं बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आपको योग की सीढ़ी पर शनैः-शनैः चरणबद्ध रूप से चढ़ना चाहिए। आपको अभ्यास को कुछ दिनों के लिए भी नहीं त्यागना चाहिए।
जो भी ध्यान करना प्रारम्भ कर रहे हों, उन्हें प्रातः काल एक घण्टे तथा सायंकाल एक घण्टे ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। अभ्यास के समय में शनैः-शनैः वृद्धि करनी चाहिए। अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि २४ घण्टे ब्रह्म-भाव रखना चाहिए। चेतना का अविरत प्रवाह होना चाहिए। आपको एक क्षण के लिए भी 'अहं ब्रह्मास्मि' अथवा दैवी उपस्थिति के विचार को भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर का विस्मरण वास्तव में मृत्यु है। यह वास्तव में आत्महत्या है। यह आत्मद्रोह है। यह सबसे बड़ा पाप है।
१३. ध्यानाभ्यास के लिए योग्यताएँ
मन को ब्रह्म के विचार से आपूरित करने से पूर्व आपको दैवी विचारों को सर्वप्रथम आत्मसात करना होगा। पहले आत्मीकरण और उसके बाद विलयन। तब एक क्षण की देरी के बिना आत्म-साक्षात्कार स्वयं ही आयेगा। इस वाक्य को सदा याद रखिए - आत्मीकरण, विलयन और फिर आत्म-साक्षात्कार।
आपको अधिक आत्म-चिन्तन, वासनाओं के उन्मूलन, इन्द्रियों पर नियन्त्रण तथा और अधिक आन्तरिक जीवन के द्वारा दृढ़, शुद्ध और अटल बनना होगा। आपको रविवार तथा छुट्टियों के प्रत्येक पल का उपयोग अपने श्रेष्ठ आध्यात्मिक लाभ हेतु करना होगा।
यदि आपने एक माह तक रसगुल्ला खाया है, तो रसगुल्ले के प्रति मानसिक आसक्ति मन में आ जाती है। इसी प्रकार यदि आप संन्यासियों की संगत में रहे, योग- वेदान्त आदि की पुस्तकें पढ़ें, तो ईश्वरीय चेतना को प्राप्त करने के लिए मन में लगाव उत्पन्न हो जायेगा। मात्र मानसिक आसक्ति आपकी बहुत अधिक सहायता नहीं कर सकेगी। इस हेतु ज्वलन्त वैराग्य, ज्वलन्त मुमुक्षुत्व, आध्यात्मिक साधना हेतु क्षमता, प्रबल तथा निरन्तर प्रयत्न और निदिध्यासन (ध्यान) की आवश्यकता है। मात्र तभी आत्मज्ञान सम्भव है।
एक सदाचारी जीवन व्यतीत करना ही मात्र भगवद्-साक्षात्कार हेतु पर्याप्त नहीं है। निरन्तर ध्यान करना आवश्यक है। एक सदाचारी जीवन धारणा तथा ध्यान हेतु मन को तैयार करता है। मात्र धारणा और ध्यान ही हैं जाते हैं। 'आत्म-साक्षात्कार की ओर ले कर
आपको गीता में प्राप्त होगा— 'मन्मनः', 'मत्परः'। ये आपको बताते हैं कि आप अपना सम्पूर्ण मन, १०० प्रतिशत मन ईश्वर को अर्पित करें। मात्र तभी आपको आत्म-साक्षात्कार प्राप्त होगा। यदि मन की एक किरण भी बाहर निकलती है, तो ईश्वर - साक्षात्कार प्राप्त करना असम्भव होगा। जिस प्रकार आप गँदले जल को फिटकरी आदि के द्वारा स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार आपको गँदले मस्तिष्क को, जो कि वासनाओं तथा मिथ्या संकल्पों से पूर्ण है, ब्रह्म-चिन्तन के द्वारा शुद्ध करना होगा। मात्र तभी सच्चा ज्ञान होगा।
जब आप ध्यान करें, आपको शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक उदाहरण देखिए, एक युवती ने बच्चे की आकांक्षा से पीपल के वृक्ष की १०८ परिक्रमाएँ कीं और तुरन्त ही अपने पेट को स्पर्श करके देखने लगी कि बालक आया या नहीं। यह तो सीधी-सीधी मूर्खता है। उसे कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करनी होगी। इसी प्रकार यदि आप कुछ समय तक नियमित ध्यान करेंगे, तो आपका मन परिपक्व होगा और आप आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। जल्दबाजी व्यर्थ है।
जब गृहस्थ यौगिक साधक ध्यान में उच्च अवस्था में पहुँच जाते हैं, यदि वे ध्यान में सच में गम्भीर हैं, तो उनको यह निर्दिष्ट किया जाता है कि उनको सभी सांसारिक गतिविधियाँ बन्द कर देनी चाहिए। उच्च साधकों के लिए काम एक बाधा है। यही कारण है कि भगवान् श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि 'एक साधु जो कि योग की खोज करता है, उसके लिए कर्म एक साधन है; किन्तु वही साधक यदि योग पर सिंहासनारूढ हो चुका है, तो उसके लिए शम साधन कहलाता है।' तब कर्म और ध्यान अम्ल और क्षार की भाँति, अग्नि और जल की भाँति अथवा प्रकाश और अँधेरे की भाँति असंगत बन जाते हैं।
आपको अपने वैराग्य, ध्यान तथा सात्त्विक गुणों जैसे धैर्य, अध्यवसाय, करुणा, प्रेम, दया, पवित्रता आदि में नित्य वृद्धि करनी चाहिए। वैराग्य तथा सद्गुण ध्यान में सहायता करते हैं। ध्यान सात्त्विक गुणों में वृद्धि करता है।
एक सर्व व्यापक ब्रह्म की भावना रखिए। इस नश्वर शरीर को एक दिखावे की भाँति अस्वीकार करें। इस भावना को सदैव बनाये रखें।
आप ध्यान के समय अपनी आँखें बन्द क्यों रखते हैं? अपनी आँखें खुली रखें। और ध्यान करें। आपको शहर की भीड़-भाड़ के मध्य अपने मन का सन्तुलन बनाये रखना चाहिए। मात्र तभी आप परिपूर्ण होंगे। प्रारम्भ में जब आप नवाभ्यासी हों, तब आप मन के विचलन को दूर करने के लिए आँखें बन्द कर सकते हैं; क्योंकि अभी आप बहुत दुर्बल हैं, किन्तु बाद में आपको आँखें खुली रख कर, यहाँ तक कि चलते समय भी ध्यान करना चाहिए। दृढ़तापूर्वक विचार करें कि यह जगत् अवास्तविक है और तब वहाँ कोई जगत् नहीं होगा। यदि आप जब आपकी आँखें खुली हों, तब भी आप आत्मा पर ध्यान कर सकते हैं, तो आप एक दृढ़ मनुष्य हैं। आप सरलता से विचलित नहीं होंगे। आप मात्र तभी ध्यान कर सकते हैं, जब आपका मन समस्त आकुलताओं से मुक्त हो।
धारणा और ध्यान में आपको अपने मन को विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षित करना होगा। मात्र तभी स्थूल मन सूक्ष्म बनेगा। जब आप जप तथा ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो सभी वृत्तियाँ सूक्ष्म रूप ग्रहण कर लेती हैं। वे तनु हो जाती हैं। उन्हें समाधि के द्वारा ज्ञानाग्नि में दग्ध करना चाहिए। मात्र तभी आप सुरक्षित रहेंगे। छिपी हुई वृत्तियाँ एक बृहत् भयंकर रूप धारण करने हेतु तैयार रहती है। आपको सदैव सावधान और जागरूक रहना चाहिए
नियमित ध्यान के द्वारा गहन विरोधी बलों के द्वारा गहन पतन को रोकें। स्पष्ट तथा सामान्य विचार के द्वारा मन के निस्देश्य भटकाव को रोकें। तुच्छ मन की झूठी बुदबुदाहट को न सुनें। अपनी आन्तरिक दृष्टि को देवी केन्द्र की ओर मोड़ें। अपनी यात्रा में आने वाले धर्कों से न घबरायें। बहादुर बनें। जब तक आप अपने परमानन्द के केन्द्र में विश्राम न कर लें, तब तक साहस के साथ आगे बढ़ते जायें।
एक बड़े शहर में रात्रि आठ बजे बहुत अधिक शोर रहता है। ९ बजे उतना शोर नहीं रहता। १० बजे शोर और भी कम रहता है। और ११ बजे यह बहुत ही कम हो जाता है। १ बजे रात को सर्वत्र शान्ति हो जाती है। इसी प्रकार योगाभ्यास के प्रारम्भ में मन में अनगिनत वृत्तियाँ रहती हैं। मन में बहुत अधिक विचलन और उत्तेजना रहती है। धीरे-धीरे विचार की लहरें शान्त हो जाती है। अन्त में मन के सभी मानसिक रूपान्तरण नियन्त्रित हो जाते हैं और योगी अनन्त शान्ति के आनन्द उपभोग करता है।
जब आप एक बड़े शहर के बाजार के बीच से गुजर रहे होते हैं, तो आपको छोटी-छोटी आवाजें सुनायी नहीं पड़तीं; लेकिन जब आप प्रातः काल अपने किसी मित्र के साथ एक शान्त कमरे में ध्यान करने के लिए बैठे होते हैं, तो आप छींकने और खाँसने की आवाजें भी पहचान सकते हैं। इसी प्रकार जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, तो आप बुरे विचारों को पहचान नहीं पाते; लेकिन जब आप ध्यान हेतु बैठते हैं, तो आप उन्हें पहचान सकने योग्य होते हैं। जब आप ध्यान के लिए बैठें, तो यदि बुरे विचार आयें, तो न घबरायें। और अधिक जप तथा ध्यान करें। वे शीघ्र चले जायेंगे।
जब आप ध्यान करें, इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले सतही जाग्रतियों को अस्वीकार कर दें। सभी अन्य बीते प्रसंगों एवं विचारों की यादों की तुलना से बचें। मन की सम्पूर्ण ऊर्जा को बिना किसी अन्य विचारों के साथ तुलना के स्वयं की आत्मा अथवा ईश्वर के एक विचार पर केन्द्रित करें।
योग के साधक को बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि यह उसे संसार के प्रलोभनों में फँसा देता है। वह अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ धन अपने पास रख सकता है। आर्थिक स्वतन्त्रता मन को आकुलताओं से मुक्त करती है और उसे निर्बाध रूप से साधना करने योग्य बनाती है।
१४. कितने घण्टे ध्यान करें
प्रारम्भ में आप प्रातः ४ से ४.३० बजे तक तथा रात्रि में ८ से ८.३० बजे तक ध्यान करें। प्रातः काल का समय ध्यान हेतु सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि मन गहन निद्रा के उपरान्त ताजा रहता है और इसके साथ ही साथ वातावरण में सात्विकता होने के कारण शरीर में सत्त्व प्रमुख रहता है। योगवासिष्ठ में ऋषि वसिष्ठ कहते हैं- "हे राम! प्रारम्भ में १/४ मन ध्यान हेतु, १/४ भाग मन मनोरंजन के लिए, १/४ भाग मन अध्ययन के लिए और १/४ भाग गुरु सेवा के लिए दो। उसके बाद ३/८ मन ध्यान के लिए, १/८ मनोरंजन के लिए, ३/८ अध्ययन के लिए और १/८ गुरु-सेवा के लिए दो ।" यहाँ मनोरंजन का अर्थ है—अन्य कार्य जैसे धोना, सफाई आदि। इसका अर्थ गोल्फ का खेल नहीं है। इसका अर्थ मन के लिए विश्राम अथवा धारणा और ध्यान के पश्चात् मन का दिशा परिवर्तन है, अन्यथा मन थकावट का अनुभव करता है और आगे काम करना अस्वीकार कर देता है। तत्पश्चात् १/२ मन ध्यान हेतु, १/२ मन अध्ययन के लिए दें। ध्यान के समय में धीरे-धीरे वृद्धि करें। जब ध्यान दो घण्टे तक होने लगे, तो इसे धीरे-धीरे एक घण्टे और बढ़ा दें। प्रात काल ४ से ५ बजे तक तथा रात्रि में ८ से ९ बजे तक। एक वर्ष पश्चात् इस समय को प्रातः डेढ़ घण्टे तथा रात को डेढ़ घण्टे तक कर दें। तीसरे वर्ष के अन्त में दो घण्टे प्रातः और दो घण्टे रात्रि कर दें। चौथे वर्ष में प्रातः तीन घण्टे तथा रात में तीन घण्टे कर दें। यह बृहत् जन-समुदाय के लिए है। एक लगनशील साधक जो दृढ़ जीवनी-शक्ति तथा सूक्ष्म बुद्धि से सम्पन्न है, वह साधना के प्रथम वर्ष में ही ६ घण्टे ध्यान कर सकता है। आपको ध्यान के साथ-साथ पवित्र ग्रन्थ जैसे योगवासिष्ठ, उपनिषद्, गीता, विवेकचूड़ामणि, अवधूत गीता आदि का स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा अध्ययन अति उत्थानकारी होता है ६ घण्टे अध्ययन और ६ घण्टे ध्यान अत्यन्त लाभकारी है। यह आपको २४ घण्टे ध्यान निदिध्यासन के लिए सहायक सिद्ध होगा।
१५. ध्यान हेतु सहायक क्रियाएँ
ध्यान में मूलबन्ध : जब आप जप करने के लिए बैठें, गुदा को संकुचित करें। इसे हठयोग में मूलबन्ध कहते हैं। यह धारणा में सहायता करता है। यह अभ्यास अपान वायु को नीचे नहीं जाने देता।
ध्यान में कुम्भक: जितनी देर आप आराम से रोक सकें, श्वास को रोके रहें। यह कुम्भक है। यह मन को स्थिर करता है और धारणा में सहायता करता है। आपको तत्काल आध्यात्मिक आनन्द की अनुभूति होगी।
यौगिक आहार : मिताहार सात्त्विक आहार लें। पेट को चावल, सब्जी, दाल तथा रोटी से अधिक मात्रा में भरने से नींद आती है और साधना में बाधा पड़ती है। एक पेटू अथवा विषयी अथवा आलसी मनुष्य ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। दूध का आहार शरीर को बहुत हल्का रखता है। इससे आप एक आसन में सरलता से और आराम से घण्टों बैठे रह सकते हैं। यदि आप दुर्बलता का अनुभव करें, तो आप एक अथवा दो दिनों तक थोड़े चावल अथवा दूध और बाजरा या कोई हल्का आहार ले सकते हैं। जो सेवा के क्षेत्र में हैं या जो व्याख्यान देते हैं अथवा जो अत्यधिक आध्यात्मिक प्रचार की गतिविधियाँ करते हैं, उनको ठोस सारभूत भोजन की आवश्यकता रहती है।
आप गीता में अक्सर निम्न शब्द पढ़ेंगे 'अनन्य चेतः - अन्य के बारे में कोई विचार नहीं; 'मत्चित्तः', 'नित्ययुक्तः', 'मन्मनः', 'एकाग्र मन' एवं 'सर्वभाव | ये शब्द बताते हैं कि आप अपना सम्पूर्ण सौ प्रतिशत मन ईश्वर को दें। मात्र तभी आपको आत्म-साक्षात्कार प्राप्त होगा। यदि एक किरण भी मन की बाहर जायेगी, तो भगवद्-चेतना प्राप्त करना असम्भव होगा।
शान्त बर्ने, स्वयं को जानें। उसे जानें। मन को उसमें विलीन कर दें। सत्य पूर्ण शुद्ध और सरल है।
१६. ध्यान हेतु आसन
प्रारम्भ में आप पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन अथवा सुखासन में आधा घण्टे तक बैठे रहें। इसके बाद इस अवधि को तीन घण्टे तक बढ़ायें। एक वर्ष में आपको आसन-सिद्धि प्राप्त हो जायेगी। कोई भी सरल और आरामदायक स्थिति आसन है।
पद्मासन
दायें पैर को बाय जाँघ पर रखें और बायें पैर को दायीं जाँघ पर रखें। घुटनों के ऊपर हाथों को रखें। नेत्रों को बन्द रखें और त्रिकुटी अथवा भ्रूमध्य पर धारणा करें। सिर गर्दन और धड़ एक सीधी रेखा में रखें। इसे कमलासन अथवा पद्मासन कहते हैं। यह ध्यान हेतु अति श्रेष्ठ है। यह गृहस्थों के लिए अत्यन्त लाभदायक है।
सिद्धासन
यह ध्यान हेतु अति श्रेष्ठ है। एक एड़ी को गुदा पर रखें, दूसरी एड़ी को जनन अंग के ऊपर रखें और हाथों को घुटने के ऊपर रखें। नेत्रों को बन्द रखें और त्रिकुटी अथवा भ्रूमध्य पर अथवा नासिकाग्र पर धारणा करें। सिर, गर्दन और घड़ एक सीधी रेखा में रखें। हाथों को पद्मासन की भाँति घुटनों के ऊपर रखें। यह आसन ब्रह्मचारियों तथा गृहस्थों के लिए अत्यन्त लाभदायक है।
स्वस्तिकासन
स्वस्तिक अर्थात् शरीर को सीधे रखते हुए आराम से बैठना। दायें पैर को बायाँ जाँघ के पास रखें और बायें पैर को ला कर दायीं जाँघ और पिण्डलियों के बीच फँसायें। यह स्वस्तिकासन है।
सुखासन
जप तथा ध्यान हेतु कोई भी आरामदायक आसन सुखासन है। यह महत्त्वपूर्ण है कि सिर, गर्दन और धड़ एक सीध में हों। यहाँ पर मैं सुखासन का एक विशेष प्रकार बता रहा हूँ जो कि वृद्ध लोगों के लिए अत्यन्त सुविधाजनक है। ५ फीट लम्बा कपड़ा लें। इसे लम्बाई में मोड़ लें। घुटनों को धड़ के बराबर रखें। कपड़े का एक सिरा बायें घुटने के पास रखें और दूसरे सिरे को बायीं ओर से घुमाते हुए पीठ की ओर ले जायें और दायें घुटने पर से होते हुए बायें घुटने के पास ला कर गाँठ बाँध लें। हाथ को घुटने के बीच में रखें। चूँकि इसमें पैरों, हाथ और रीढ़ की हड्डी को सहारा मिल जाता है, इस कारण इस आसन में लम्बे समय तक आराम से बैठा जा सकता है।
आसनों के लाभ
आसन अनेक रोगों को जैसे बवासीर, अजीर्ण, कब्ज को दूर करते हैं तथा अत्यधिक रजोगुण को रोकते हैं। शरीर को आसनों से सही विश्राम प्राप्त होता है। यदि आप आसनों में स्थापित हैं, यदि आप अपने आसन में दृढ़ हैं, तब आप सरलता से प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यह पतंजलि के राजयोग अथवा अष्टांगयोग का तीसरा अंग है।
सर्वप्रथम इसमें आत्म-संयम अथवा अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य आदि का अभ्यास है। तत्पश्चात् वहाँ धार्मिक नियम जैसे शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय आदि हैं। इसके बाद आसन आते हैं। जब आसन स्थिर हो जाता है, तो आपको शरीर का अनुभव नहीं होता। जब आप आसनों में प्रवीण हो जाते हैं, तो तब आपको द्वन्द्व जैसे शीत अथवा गर्मी आदि प्रभावित नहीं करते। आपको आसन खाली पेट करने चाहिए; किन्तु आप आसन करने के पहले एक छोटा कप दूध, चाय अथवा काफी ले सकते हैं। आसन शरीर को स्थिर करते हैं। बन्ध तथा मुद्राएँ शरीर को दृढ़ बनाते हैं। प्राणायाम शरीर को हल्का बनाता है। नाड़ी-शुद्धि से मन की स्थिरता आती है। इसकी प्राप्ति होने पर आपको अपने मन को ब्रह्म पर एकाग्र करना चाहिए। ऐसा करने पर ही ध्यान स्थिरतापूर्वक सरलता से और आनन्दपूर्वक होता है। ध्यान, धारणा और जप के लिए पद्मासन अथवा सिद्धासन निर्दिष्ट है। सामान्य स्वास्थ्य एवं ब्रह्मचर्य पालन के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन उत्तम हैं।
१७. ध्यान में नियमितता
जो भी आध्यात्मिक साधना आप करें, चाहे वह जप या आसनों का अभ्यास या सगुण मूर्ति पर स्थूल ध्यान अथवा प्राणायाम हो, उसे प्रतिदिन नियमित और क्रमबद्ध रूप से करें। इस अभ्यास के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अमरता प्राप्त होगी और तब सभी कामनाएँ समाप्त हो जायेंगी। आपको नित्य तृप्ति प्राप्त होगी।
मेरे प्रिय मित्र! ध्यान करें, ध्यान करें। धारणा करें, धारणा करें। आलस्य के कारण एक दिन भी न चूकें। आलस्य साधक का महान् शत्रु है। जीवन क्षणिक है, समय बीता जा रहा है और आध्यात्मिक पथ में बहुत-सी बाधाएँ हैं। प्रयत्न और प्रार्थना के द्वारा इनको एक-एक करके दूर करें। यदि आप गम्भीर हैं, तो आपको भीतर से, बाहर से, सूक्ष्म लोक के सहायता करने वालों से, संसार के सभी भागों में बिखरे जीवन्मुक्तों तथा चिरंजीवियों—–श्री व्यास, वसिष्ठ, कपिल मुनि से, गिरनार पर्वत के दत्तात्रेय भगवान् से, पोडिया पर्वत तिरुनेलवेली के अगस्त्य मुनि से सहायता प्राप्त होगी।
जिस प्रकार आप चार बार—प्रातः, मध्याह्न, सायं और रात्रि को भोजन करते हैं, इसी प्रकार यदि आप शीघ्र आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको दिन में चार बार ध्यान करना चाहिए। आपको अपने ध्यान में नियमित होना चाहिए।
जिस प्रकार भाँग, अफीम अथवा शराब यदि आप थोड़ी भी मात्रा में लेते हैं, आपको नशा देती है और यह नशा कुछ घण्टों तक बना रहता है। उसी प्रकार यदि तो आप आधा घण्टे भी नियमित ध्यान करते हैं, नियमित ध्यान से प्राप्त होने वाला भगवद्-प्रेम कई घण्टों तक बना रहता है, इसलिए आप ध्यान में नियमित रहें।
जब आप ध्यान करते हैं, जब आप सात्त्विक गुणों का विकास करते हैं, तो मन में आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। यदि आप ध्यान में नियमित नहीं हैं, यदि आपका वैराग्य क्षीण हो गया है, यदि आप असावधान हो गये हैं, तो अशुद्ध विचारों तथा बुरी वासनाओं की बाढ़ से आध्यात्मिक मार्ग धुल कर बह जायेगा। इसलिए ध्यान में नियमितता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।
जब आप ध्यान, जप, कीर्तन, प्राणायाम अथवा चिन्तन का अभ्यास करते हैं, तो सांसारिक विचार, अभिलाषाएँ तथा वासनाएँ दब जाती हैं। यदि आप ध्यान में नियमित नहीं रहेंगे और यदि आपका वैराग्य क्षीण हो गया है, तो वे पुनः प्रकट होने का प्रयास करती हैं। इसलिए आप ध्यान में नियमित रहें और अधिक कठोर साधना करें। अधिक वैराग्य का अर्जन करें। सांसारिक विचार, अभिलाषाएँ तथा वासनाएँ तनु हो जायेंगी और अन्ततः नष्ट हो जायेंगी।
अध्याय ४
ध्यान का अभ्यास
१. ध्यान का व्यावहारिक रूप
यह संसार कष्टों और दुःखों से परिपूर्ण है। यदि आप इस संसार के दुःख तथा कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है, जो कि अनन्त शान्ति और परमानन्द लाता है। ध्यान आपको सम्पूर्ण अनुभव अथवा प्रत्यक्ष अन्तर्ज्ञान हेतु तैयार करता है। एक ही वस्तु अथवा ईश्वर अथवा आत्मा के निरन्तर विचार को ध्यान कहते हैं। ध्यान देवत्व के लिए मार्ग है। यह ब्रह्मलोक का राज मार्ग है। यह रहस्यमय सीढ़ी है जो कि पृथ्वी से स्वर्ग तक (वैकुण्ठ, कैलास अथवा ब्रह्म), असत्य से सत्य तक, अन्धकार से प्रकाश तक, दुःख से सुख तक, बेचैनी से शान्ति तक, अज्ञानता से ज्ञान तक और नश्वरता से अमरता तक पहुँचती है।
सत्य ब्रह्म है। सत्य आत्मा है। आप ध्यान के बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ध्यान की विधि साधक के द्वारा अपनाये गये पथ पर निर्भर करती है। एक भक्त अपने इष्टदेवता के रूप पर सगुण ध्यान का अभ्यास करता है। एक हठयोगी चक्रों तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं का ध्यान करता है। एक ज्ञानयोगी अपनी आत्मा पर ध्यान करता है। वह अहंग्रह उपासना करता है। एक राजयोगी उस पुरुष का ध्यान करता है जो कष्टों तथा कामनाओं से प्रभावित नहीं होता।
मन उस विषय के रूप को ग्रहण कर लेता है, जिसका उसे बोध होता है। ऐसा होने के बाद ही उस विषय को देखना सम्भव है। एक भक्त निरन्तर अपने इष्टदेवता के रूप का ध्यान करता है। उसका मन सदैव इष्टदेवता के रूप को ग्रहण करता है। जब वह अपने ध्यान में स्थापित हो जाता है, जब वह पराभक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो वह सर्वत्र अपने इष्टदेवता का दर्शन करता है। नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं। एक कृष्ण भगवान् का भक्त सर्वत्र मात्र भगवान् कृष्ण को ही देखता है और गीता में वर्णित स्थिति 'वासुदेवः सर्वमिति —— प्रत्येक वस्तु वासुदेव ही है' का अनुभव करता है एक ज्ञानी अथवा वेदान्ती सर्वत्र अपनी आत्मा के दर्शन करता है। उसके दृष्टिकोण से समस्त नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं। वह उपनिषदों के ऋषियों के कथन 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म-सभी वास्तव में ब्रह्म हैं' का अनुभव करता है।
यदि आप आत्म-साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। जब तक मन मुक्त नहीं होगा तथा सभी कामनाओं, अभिलाषाओं, चिन्ताओं, मोह, अहंकार, वासना तथा आसक्ति को दूर नहीं किया जायेगा, तब तक उस परम धाम के भीतर जो कि परम शान्ति तथा शुद्ध आनन्द के स्रोत का स्थान है, प्रवेश करना सम्भव नहीं होगा। एक पेटू, विषयी अथवा आलसी मनुष्य ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। जिसने अपनी जिह्वा तथा अन्य अंगों पर नियन्त्रण कर लिया है, जो विवेकी है, जो आहार और शयन में संयमित है, जिसने स्वार्थ, वासना, लोभ तथा क्रोध का नाश कर लिया है, वह ध्यान का अभ्यास कर सकता है और समाधि में सफलता प्राप्त करता है।
यदि आपके मन में विक्षेप होगा, तो आप मन की शान्ति नहीं प्राप्त कर सकते और ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते। विक्षेप का अर्थ है मन का भटकना। विक्षेप रजोगुण है। विक्षेप तथा कामनाएँ मन में एक साथ उपस्थित रहती हैं। यदि आप वास्तव में विक्षेपों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको वैराग्य और ईश्वर के प्रति आत्म-समर्पण के द्वारा सभी नश्वर कामनाओं तथा आकांक्षाओं को नष्ट कर देना चाहिए।
यदि आप हरी लकड़ी में आग लगायेंगे, तो वह नहीं जलेगी; यदि आप सूखी लकड़ी में आग लगायेंगे, तो यह तुरन्त अग्नि पकड़ लेगी और जल जायेगी। इसी प्रकार जिनके मन शुद्ध नहीं हैं, वे ध्यान की अग्नि जलाने के योग्य नहीं हैं। जब वे ध्यान हेतु बैठेंगे, तो सोते रहेंगे या स्वप्न देखेंगे अथवा हवाई किले बनायेंगे; लेकिन जिन्होंने जप, ध्यान, सेवा, दान और प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध कर लिया है, वे ध्यान में बैठने के बाद शीघ्र ही ध्यान में प्रविष्ट हो जाते हैं। शुद्ध और परिपक्व मन तत्काल ध्यान की अमि से प्रज्वलित हो उठता है।
मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। जिस प्रकार आप जमीन को जोतने बोने के बाद, खरपतवार तथा काँटे उखाड़ कर और पौधों को जल से सींच कर एक बगीचे में फूल और फल उगा सकते हैं, उसी प्रकार आप अपने मन के बगीचे में मन की अशुद्धियों जैसे वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को दूर करके तथा इसमें दैवी विचारों का जल सींच कर भक्ति के फूल उगा सकते हैं। काँटे और झाड़ियाँ वर्षा ऋतु में उगते हैं और ग्रीष्म ऋतु में अदृश्य हो जाते हैं; किन्तु उनके बीज जमीन में ही पड़े रहते हैं। जैसे ही वर्षा होती है, ये बीज पुनः अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार मन की वृत्तियाँ चेतन मन की सतह पर प्रकट होती है, तत्पश्चात् अदृश्य हो जाती है और एक सूक्ष्म बीज अवस्था संस्कार रूप को ग्रहण कर लेती है। संस्कार आन्तरिक अथवा बाह्य उत्प्रेरक के द्वारा वृत्ति बन जाते हैं। जब बगीचा साफ होगा और वहाँ काँटे और झाड़ियाँ नहीं होंगे, तो वहाँ आप उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जब मन शुद्ध होगा तथा वासना और क्रोध आदि से मुक्त होगा, तो आपको गहन ध्यान का फल प्राप्त होगा। इसलिए सर्वप्रथम मन की अशुद्धियों को स्वच्छ करें। फिर ध्यान की विद्युत् स्वयं प्रवाहित होगी।
यदि आप बगीचे को सदैव स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो आपको न केवल काँटे और झाड़ियों को ही उखाड़ना होगा, बल्कि आधारभूत भूमि के नीचे दबे हुए उन बीजों को भी निकाल फेंकना होगा, जो कि वर्षा ऋतु में अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप समाधि में प्रवेश करना चाहते हैं अथवा मुक्ति या पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मन की वृत्तियों अथवा बड़ी तरंगों को ही नष्ट नहीं करना होगा, बल्कि आधारभूत उन संस्कारों को भी नष्ट करना होगा जो कि जन्म-मृत्यु के बीज हैं और बार-बार वृत्तियों को जन्म देते हैं।
बिना ध्यान की सहायता के आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बिना इसकी सहायता के आप दैवी स्थिति में विकास नहीं कर सकते। बिना इसके आप स्वयं को मन की जकड़न से मुक्त नहीं कर सकते। इसके बिना आप अमरता नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आप ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे, तो आत्मा का परम वैभव एवं परम सौन्दर्य आपसे छुपा रहेगा। ध्यान के अभ्यास के द्वारा उस आवरण को चीर दें, जो आत्मा को आवृत किये है। निरन्तर ध्यान के द्वारा आप उन पाँचों कोशों को चीर दें, जो कि आत्मा को ढाँके हुए हैं और तत्पश्चात् जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें।
२. ध्यान में सच्चा विश्राम
थकी हुई इन्द्रियों को विश्राम की आवश्यकता होती है। इसी कारण रात्रि में नींद आती है। गति और विश्राम जीवन की एक के बाद एक चलने वाली गतिविधियाँ हैं। मन वासना के बल पर इन्द्रियों के लोक में भ्रमण करता है। मैं दृढतापूर्वक कहता हूँ कि दृढ़ सुषुप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। स्वप्न में भी मन की सूक्ष्म गतिविधि चलती रहती है। इस कारण आपको निद्रा में भी सच्चा विश्राम प्राप्त नहीं होता। सच्चा विश्राम मात्र ध्यान में ही सम्भव है। मात्र ध्यानयोगी जो ध्यान का अभ्यास करते हैं, वे ही ध्यान में सच्चे विश्राम का अनुभव करते हैं। ध्यान की अवधि में मन पूर्ण एकाग्र होता है। यह विषयों से बहुत दूर रहता है और आत्मा के बहुत पास रहता है। ध्यान के समय विषय की अनुपस्थिति होने के कारण राग-द्वेष की तरंगें नहीं होतीं। परिणाम स्वरूप वहाँ स्थायी सच्चे आध्यात्मिक आनन्द के साथ सच्चा और पूर्ण विश्राम होता है। आप स्वयं अनुभव करें, तब आप मेरे साथ सहमत होंगे। बनारस के एक हठयोगी जो कि वायु में तैरते थे, वे रात्रि में सोते नहीं थे। वे सारी रात आसन में बैठते थे। उन्हें ध्यान से सच्चा विश्राम प्राप्त होता था। वे नींद से पूर्ण मुक्त थे। आप अपने अभ्यास के प्रारम्भ में पूर्ण विश्राम का आनन्द नहीं ले पायेंगे; क्योंकि तब इच्छा-शक्ति और स्वभाव के मध्य, पुराने संस्कारों और नवीन संस्कारों के मध्य, पुरानी आदतों और नयी आदतों के मध्य, पुरुषार्थ और पुराने व्यवहार के मध्य संघर्ष होगा। मन विद्रोह करेगा। जब मन तनु हो जायेगा, जब आप तनुमानसी अवस्था में तृतीय ज्ञान भूमिका में पहुँच जायेंगे और तब आप ध्यान में अच्छा विश्राम प्राप्त करेंगे। आप अपनी नींद धीरे-धीरे तीन अथवा चार घण्टों तक सीमित कर सकेंगे।
३. नेत्र बन्द कर मानसिक चित्रण करना
अपने इष्टदेवता के चित्र को कुछ मिनटों तक अपलक देखें और नेत्रों को बन्द कर लें। इसके बाद मानसिक रूप से चित्र को देखने का प्रयास करें। आपको भगवान् का चित्र एकदम स्पष्ट दिखायी देना चाहिए। जब यह धुँधला पड़ने लगे, तो नेत्रों को खोल कर चित्र को पुनः देखें। इस क्रिया-विधि को ४ या ५ बार दोहरायें। कुछ माह के अभ्यास के बाद आप अपने इष्टदेवता के चित्र को मानसिक रूप से भी स्पष्ट रूप से देख सकेंगे।
यदि आप सम्पूर्ण चित्र को न देख सकें, तो चित्र के किसी एक भाग को देखने का प्रयास करें। एक अस्पष्ट चित्र बनाने का प्रयास करें, बार-बार के अभ्यास से यही चित्र एक स्पष्ट चित्र का रूप ग्रहण कर लेगा। यदि आपको इसमें कठिनाई हो, तो आप मन को हृदय में प्रकाशित ज्योति पर एकाग्र करने का प्रयास करें और इस ज्योति को देवी अथवा देवता के रूप में लें।
यदि आप स्पष्ट रूप से चित्र को न देख सकें, तो चिन्ता न करें। अपने अभ्यास को नियमित रूप से करते रहें। आप विकास करेंगे। जो चाहिए, वह है ईश्वर के प्रति प्रेम । इसका अधिकाधिक अर्जन कीजिए। इसका निरन्तर सहज रूप से प्रवाह होने दीजिए । यह मानसिक रूप से चित्रण करने से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
४. ध्यानयोग
प्रारम्भ में आप दो बार ध्यान कर सकते हैं—४ से ६ बजे तक सुबह और ७ से. ८ बजे तक रात में। जब आप ध्यान में आगे बढेंगे. तो आप अपने सामान्य ज्ञान तथा विवेक का प्रयोग करके प्रत्येक बैठक के समय में शनैः-शनैः वृद्धि कर सकते हैं तथा एक तीसरी बैठक सुबह १० से ११ बजे तक और शाम को ४ से ५ बजे तक कर सकते हैं।
योगवासिष्ठ में आप पायेंगे — “मन का दो भाग आनन्द के विषयों से, एक भाग दर्शन से तथा शेष भाग गुरु के प्रति भक्ति से भरना चाहिए। थोड़ा विकास होने पर उसे मन का एक भाग आनन्द के विषयों से भरना चाहिए, दो भाग गुरु के प्रति भक्ति से तथा शेष एक भाग दर्शन के अर्थ में अन्तर्दृष्टि को प्राप्त करके उससे भरना चाहिए। जब कोई एक बार दक्षता प्राप्त कर ले, तो उसे प्रतिदिन अपने मन के दो भाग को दर्शन एवं परम वैराग्य से और शेष दो भागों को ध्यान तथा गुरु के प्रति समर्पण युक्त सेवा से भरना चाहिए। यह आपको २४ घण्टे ध्यान हेतु प्रेरित करेगा। जो नवाभ्यासी इस प्रकार अभ्यास करता है, वह सही प्रकार साधना कर रहा है।"
ध्यान के अपने प्रिय आसन में बैठ कर, सिर और धड़ को एक सीध में रख कर नेत्रों को बन्द कर लें और नासिका के अग्रभाग, भ्रूमध्य, हृदय-कमल अथवा सिर के शीर्ष भाग पर धारणा करें। एक बार यदि आपने धारणा हेतु केन्द्र का निर्धारण कर लिया तो अन्त तक उससे जोंक की भाँति चिपके रहें। जैसे यदि आपने धारणा हेतु हृदय-कमल का चुनाव किया है, तो कभी भी इसे न बदलें। ऐसा करने पर ही आप शीघ्र प्रगति की अपेक्षा कर सकते हैं।
ध्यान दो प्रकार का होता है—सगुण और निर्गुण । भगवान् श्री कृष्ण, भगवान् शिव, भगवान् राम अथवा भगवान् ईसामसीह पर ध्यान सगुण ध्यान कहलाता है। यह रूप अथवा गुणों पर ध्यान है। इसके साथ-साथ भगवान् के नाम का जप भी किया जा सकता है। यह भक्तों की विधि है। आत्मा की यथार्थता पर ध्यान निर्गुण ध्यान कहलाता । यह वेदान्तियों की विधि है। 'ॐ', 'सोऽहं', 'शिवोऽहं', 'अहं ब्रह्मास्मि एवं है। 'तत्त्वमसि' पर ध्यान निर्गुण ध्यान है।
ज्ञानी जन अहंकार की गाँठ को निरन्तर ध्यान की तेज धार वाली तलवार से काट डालते हैं। उसके बाद आत्मा का परम ज्ञान अथवा पूर्ण ज्ञान या आत्म-साक्षात्कार आता है। मुक्त ऋषि को न तो सन्देह होता है और न ही भ्रम। उसके कर्मों के सभी बन्धन कट जाते हैं। इसलिए सदा ध्यान में लगे रहिए। यह अनन्त आनन्द के लोक के द्वार को खोलने की कुंजी है। यह प्रारम्भ में अरुचिकर और थका देने वाला अवश्य प्रतीत होता है; क्योंकि मन प्रतिक्षण लक्ष्य से भाग जाता है, लेकिन कुछ समय बाद यह लक्ष्य पर केन्द्रित हो जाता है। आप देवी आनन्द में लीन हो जाते हैं।
जब आपको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो, तो डरें नहीं। यह प्रचुर आनन्द का नवीन अनुभव होगा। वापस न लौटें। ध्यान को न त्यागें।
आपको वहाँ रुकना नहीं है। आपको अभी भी आगे जाना है। यह सत्य की झलक मात्र है। यह सम्पूर्ण अनुभव नहीं है। यह परम साक्षात्कार नहीं है। यह मात्र एक नया मंच है। आगे चढ़ने का प्रयत्न करें। भूमा अथवा अनन्त तक पहुँचें। अब आप सभी प्रलोभनों के लिए दुर्भेद्य हैं। आप अमरता के मधु को गहरे तक पियेंगे। यह अन्तिम स्थिति है। अब आप अनन्त विश्राम कर सकते हैं। अब आपको और अधिक ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। यह अन्तिम लक्ष्य है।
आपके स्वयं के भीतर अद्भुत शक्तियाँ एवं गुप्त योग्यताएँ हैं, जिनके बारे में वास्तव में आपने कभी कोई विचार नहीं किया। आपको इन गुप्त शक्तियों और क्षमताओं को ध्यान तथा योग के अभ्यास से जगाना चाहिए। आपको अपनी संकल्प शक्ति का विकास करना चाहिए और अपनी इन्द्रियों तथा मन को नियन्त्रित करना चाहिए। आपको स्वयं को शुद्ध करना चाहिए और नित्य ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही आप परम पुरुष अथवा देव पुरुष बन सकेंगे।
प्रत्येक मनुष्य के भीतर अनेक योग्यताएँ एवं क्षमताएँ हैं। वह शक्ति और ज्ञान का भण्डार है। जैसे-जैसे वह विकास करता है, वह नयी शक्तियों, नयी योग्यताओं और नये गुणों को अनावृत करता है। अब वह अपने वातावरण को परिवर्तित कर सकता है और अन्यों को प्रभावित कर सकता है। वह अन्यों के मनों को वशीभूत कर सकता है। वह आन्तरिक और बाह्य प्रकृति को विजित कर सकता है। वह परम चेतनावस्था में प्रवेश कर सकता है।
यदि दीपक की बाती छोटी होगी, तो उसकी लौ भी छोटी होगी। यदि दीपक की बाती बड़ी होगी, तो उसका प्रकाश भी शक्तिशाली होगा। इसी प्रकार यदि जीव शुद्ध यदि उसने ध्यान का अभ्यास किया है, तो आत्मा का प्राकट्य अथवा अभिव्यक्ति भी शक्तिशाली होगी। वह अधिक प्रकाश विकिरित करेगा। यदि वह अविकसित एव अशुद्ध होगा, तो वह जले हुए कोयले की भाँति होगा। यदि दीपक की बाती बड़ी होगी, तो उसका प्रकाश भी शक्तिशाली होगा; इसी प्रकार जितनी शुद्ध आत्मा होगी, उसका उतना ही महान् आध्यात्मिक उत्थान होगा।
यदि चुम्बक शक्तिशाली होगा, तो यह लोहे के कर्णो जब वे अधिक दूरी पर भी रखे हुए होंगे, तो भी प्रभावित कर सकेगा।
इसी प्रकार यदि योगी उच्च है, तो वह अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों पर अधिक प्रभाव डाल सकेगा। वह अपना प्रभाव लोगों पर तब भी डाल सकेगा, जब कि वे उससे कहीं दूरस्थ स्थान पर निवास कर रहे होंगे।
ध्यान के समय नोट करें कि आप कितनी देर तक सांसारिक विचारों को रोक सकते हैं। अपने मन को देखें। यदि यह समय बीस मिनट है, तो इसकी अवधि तीस मिनट या इसी प्रकार से और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। मन को बार-बार भगवान् के विचारों से आपूरित करने का प्रयास करें।
“चाहे कोई मनुष्य १००० वर्षों तक एक पैर पर खड़े रह कर तपस्या करे, तो भी यह ध्यान योग के १/१६ वें भाग के भी बराबर नहीं होगा।" (पिंगल उपनिषद्)
आपको अपने वैराग्य, ध्यान तथा सद्गुणों जैसे धैर्य, अध्यवसाय, करुणा, प्रेम, दयालुता आदि में नित्य वृद्धि करनी चाहिए। वैराग्य तथा सद्गुण ध्यान में सहायता करते हैं तथा ध्यान सद्गुणों में वृद्धि करता है।
ध्यान के अभ्यास से मन, मस्तिष्क एवं नाड़ी-तन्त्र में अनेक परिवर्तन होते हैं। नवीन नाड़ी तरंगों, नवीन स्पन्दन, नयी लीकों, नयी गलियों, नवीन कोशिकाओं, नवीन तरंगों का निर्माण होता है। सम्पूर्ण मन तथा नाड़ी-तन्त्र का पुनर्निर्माण होता है। आपको एक नया हृदय, नया मन, नवीन स्पन्दन, नवीन भाव, विचार तथा कार्य करने का नया तरीका तथा विश्व के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण (जैसे भगवान् प्रकट रूप में हो) प्राप्त होता है।
ध्यान के समय आप भावोत्कर्ष में होते हैं। यह पाँच प्रकार का होता है—न्यून भावोन्माद, क्षणिक भावोन्माद, हर्षोन्माद, प्रलयकारी भावोन्माद तथा सर्वव्यापक भावोन्मादा न्यून भावोन्माद में शरीर के रोयें खड़े हो जाते हैं। क्षणिक भावोन्माद में जैसे बार-बार बिजली चमकती है, ऐसा अनुभव होता है। जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर बार-बार लहरें टूटती हैं, प्रलयकारी भावोन्माद उसी प्रकार शरीर पर तीव्रता से आक्रमण करता है और टूट जाता है। हर्षोन्माद अत्यन्त शक्तिशाली होता है और शरीर को ऊपर उठा लेता है। जब सर्वव्यापक भावोन्माद आता है, तो सम्पूर्ण शरीर पूर्णतया आवेशित हो जाता है और फूले हुए गुब्बारे की तरह आपे से बाहर हो जाता है।
"जो भी वह योगाभ्यासी अपनी आँखों से देखता है, उसे आत्मा की भाँति मानता है। जो भी वह अपनी जिह्वा से चखता है, उसे आत्मा की भाँति मानता है। जो भी वह अपनी नासिका से सूँघता है, वह उसे आत्मा की भाँति मानता है। जो भी वह अपने कानों से सुनता है, उसे आत्मा की भाँति मानता है। जो भी वह अपनी त्वचा से स्पर्श करता है, उसे आत्मा की भाँति मानता है। योगी को प्रतिदिन एक यम अर्थात् ३ घण्टे तक इस प्रकार बड़े ही प्रयत्नपूर्वक अपनी इन्द्रियों को अथक रूप से तृप्त करना चाहिए। जब योगी अपने प्रयासों में पूरी तरह डूब जाता है, तो उसे अनेक प्रकार की सिद्धियाँ — जैसे दूर-दृष्टि, दूर-श्रवण, एक ही क्षण में स्वयं को कहीं भी दूर स्थान में पहुँचा देना, महान् वाक्- शक्ति, कोई भी रूप धारण करने की सामर्थ्य, अदृश्य हो जाने की सामर्थ्य, लोहे को स्वर्ण में बदलने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है।" (योगतत्त्व उपनिषद्)
मात्र सदाचारी जीवन बिताना ही भगवद्-साक्षात्कार हेतु पर्याप्त नहीं है। मन की एकाग्रता अत्यन्त आवश्यक है। एक उत्तम सदाचारी जीवन मन को धारणा तथा ध्यान हेतु एक उपयोगी उपकरण की भाँति तैयार करता है, जो कि आत्म-साक्षात्कार, भगवद्-साक्षात्कार हेतु प्रेरित करता है।
५. एकान्त और ध्यान
राजा जनक, एकनाथ और कई अन्य लोगों ने इस जगत् में निवास करते हुए आध्यात्मिक साधना करते हुए ही साक्षात्कार प्राप्त किया था। गीता का मुख्य ज्ञान यह है कि जगत् के भीतर और जगत् के द्वारा साक्षात्कार करो। ऐसा कर सकना सम्भव है; किन्तु यह अधिकांश लोगों के लिए सम्भव नहीं है। यह कहना सरल है, किन्तु इसे करना कठिन है। ऐसे कितने जनक और एकनाथ आपके पास हैं? वे लोग वास्तव में योगभ्रष्ट थे। यह बृहत् जन-समुदाय के लिए असम्भव है।
भगवान् ईसामसीह के बारे में १८ वर्षों तक किसी को पता नहीं था। बुद्ध ८ वर्षों तक उरुवला वन में एकान्त वास में रहे। स्वामी रामतीर्थ ने ब्रह्मपुरी वन में २ वर्षों तक एकान्त-वास किया। श्री अरविन्द ने हमें शिक्षा दी कि कर्म करते हुए भी व्यक्ति साक्षात्कार कर सकता है; किन्तु उन्होंने स्वयं को एक कमरे में ४० वर्षों तक बन्द रखा। अनेक लोगों ने साधना काल में एकान्त-वास किया। आप साधना का प्रारम्भ संसार में रहते हुए कर सकते हैं; किन्तु जब आप थोड़ी प्रगति कर लें, तो आपको एक ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ आपको आध्यात्मिक स्पन्दन और एकान्त प्राप्त हो सके।
कुछ लोगों की संकल्प-शक्ति अत्यन्त दुर्बल होती है; क्योंकि उन्होंने युवावस्था में स्कूलों अथवा महाविद्यालयों में किसी प्रकार का धार्मिक अनुशासन अथवा प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है और वे भौतिक प्रभावों के जंजाल में फँसे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए आवश्यक है कि वे कठोर जप तथा निर्बाध ध्यान हेतु कुछ सप्ताहों, महीनों अथवा वर्षों के लिए एकान्त-वास के लिए चले जायें।
शान्त ध्यान के द्वारा उमड़ते आवेगों, भावनाओं, सहज प्रवृत्तियों तथा तरंगों को शान्त करें। शनैः-शनैः क्रमबद्ध अभ्यास के द्वारा आप अपनी भावनाओं को नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी सांसारिक प्रकृति को दैवी प्रकृति में पूर्ण रूपान्तरित कर सकते हैं। आप ध्यान के अभ्यास से नाड़ी तरंगों, नाड़ियों, पेशियों, पंच कोशों, आवेगों आदि पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर सकते हैं।
जिनके पुत्र अपने जीवन में स्थापित हो गये हों, जो नौकरी से सेवा-निवृत्त हो चुके हों, जिन्हें इस संसार के प्रति कोई बन्धन अथवा मोह न हो, वे ४ या ५ वर्षों तक एकान्त वास कर सकते हैं तथा शुद्धिकरण एवं आत्म-साक्षात्कार हेतु प्रबल ध्यान और तप कर सकते हैं। यह उच्च शिक्षा अथवा स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेने के समान है। जब तपस्या पूर्ण हो जाये, जब उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाये, तो उनको बाहर आना चाहिए और अपने ज्ञान तथा आनन्द में अन्यों को साझीदार बनाना चाहिए। उनको व्याख्यानों, प्रवचनों आदि के द्वारा अथवा हृदय से हृदय के वार्तालाप के द्वारा अपनी क्षमता एवं स्थिति के अनुसार आत्मज्ञान का प्रचार करना चाहिए।
योग-प्रवृत्ति तथा आध्यात्मिक झुकाव वाले गृहस्थ को अपने स्वयं के घर में एक शान्त कमरे में अथवा छुट्टियों में किसी पवित्र नदी के किनारे एकान्त स्थान पर अथवा यदि वह सम्पूर्ण समय का साधक है या वह सेवा-निवृत्त हो चुका है, तो सम्पूर्ण वर्ष तक ध्यानाभ्यास करना चाहिए।
यदि आप ध्यान के अभ्यास के लिए एकान्त वास हेतु जाना चाहते हैं, यदि आप गृहस्थ हैं और प्रबल साधना हेतु आध्यात्मिक आकांक्षा रखते हैं, तो आपको अपने परिवार जनों से एकदम से सम्बन्ध नहीं तोड़ना चाहिए। अचानक सांसारिक बन्धनों को तोड़ देना आपको मानसिक दुःख देगा तथा आपके परिवार जनों को झटका लगेगा। आपको सम्बन्ध धीरे-धीरे तोड़ना चाहिए। प्रारम्भ में एक सप्ताह अथवा एक माह के लिए एकान्त-वास हेतु जायें। उसके बाद धीरे-धीरे समयावधि में वृद्धि करें। तब उनको अलगाव का अनुभव नहीं होगा।
साधक को आशा, कामना तथा लोभ से मुक्त होना चाहिए, मात्र तभी वे । एक स्थिर मन प्राप्त कर सकेंगे। आशा, कामना तथा लोभ मन को सदैव बेचैन और उपद्रवी रखते हैं। वे शान्ति तथा आत्मज्ञान के शत्रु हैं। उसके पास बहुत-सा सामान भी नहीं होना चाहिए। उसे मात्र वे ही चीजें रखनी चाहिए, जो शरीर के निर्वाह के लिए अनिवार्य हैं। यदि उसके पास बहुत-सा सामान होगा, तो मन हमेशा उन चीजों के बारे में विचार करता रहेगा और उनकी सुरक्षा हेतु प्रयत्न करेगा। जो एकान्त-वास में ध्यान में शीघ्र प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें पत्र-व्यवहार, समाचार-पठन अथवा पारिवारिक सदस्यों के बारे में विचार करना आदि के द्वारा संसार से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए।
जिसने अपनी आवश्यकताओं को कम कर लिया है, जिसे संसार के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है, जो विवेक वैराग्य तथा मोक्ष की ज्वलन्त आकांक्षा से है. युक्त जिसने कई महीनों तक मौन का पालन किया है, वह एकान्त-वास हेतु उपयुक्त है।
साधक को शान्त रहना चाहिए। दैवी प्रकाश मात्र शान्त मन में ही आता है। शान्त भाव वासनाओं, कामनाओं तथा आकांक्षाओं के उन्मूलन से प्राप्त होता है। उसे निर्भय भी होना चाहिए। यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। एक भीरु साधक आत्म-साक्षात्कार से बहुत अधिक दूर है।
साधक को अपने शरीर की आवश्यकताओं के प्रति चिन्तित नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रत्येक चीज भगवान् देता है। प्रत्येक चीज माँ प्रकृति के द्वारा पूर्व नियोजित है। प्रकृति स्वयं ही प्रत्येक की शारीरिक आवश्यकता का स्वयं व्यक्ति की अपेक्षा बड़ी ही सावधानी और कुशलतापूर्वक ध्यान रखती है। प्रकृति को स्वयं ही ज्ञान है कि कब, क्या और किस प्रकार प्रदान करना है। माँ के रहस्यमय तरीकों को जानें और बुद्धिमान् बनें। उनकी अनूठी दयालुता, कृपा और करुणा के प्रति सदैव कृतज्ञ रहें।
वीर्य नाड़ियों तथा मस्तिष्क को लचीला बनाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जिसने इस जीवनी-शक्ति को ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा संरक्षित किया है तथा इसे ओज-शक्ति के रूप में रूपान्तरित किया है, वह लम्बे समय तक स्थिर ध्यान का अभ्यास कर सकता है। ऐसा साधक ही मात्र योग की सीढ़ी पर चढ़ सकता है। बिना ब्रह्मचर्य पालन के तनिक भी आध्यात्मिक प्रगति सम्भव नहीं है। ब्रह्मचर्य वह नींव है, जिस पर ध्यान और समाधि का भव्य भवन निर्मित किया जा सकता है। अनेक लोग अन्धे हो कर उत्तेजना में अपनी बुद्धि-शक्ति को खो बैठते हैं और इस जीवनी-शक्ति-वास्तव में एक महान् आध्यात्मिक कोष का अपव्यय करते हैं। वास्तव में वे बड़े ही दयनीय हैं। ऐसे लोग योग में किसी प्रकार की सारभूत प्रगति नहीं कर पाते।
ध्यान का गहन और निरन्तर अभ्यास आरम्भ करने से पूर्व आपको आसनों का नियमित अभ्यास करके शरीर पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त करना चाहिए। एक स्थिर आसन के बिना आप ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकेंगे। यदि शरीर अस्थिर है, तो मन भी अस्थिर होगा। शरीर और मन के मध्य एक अन्तरंग सम्बन्ध है। आपको शरीर को तनिक भी हिलाना नहीं चाहिए। आपको नित्य अभ्यास के द्वारा आसन पर निपुणता (आसन- जय) प्राप्त करनी चाहिए। आपको एक मूर्ति अथवा चट्टान की भाँति स्थिर होना चाहिए। यदि आप शरीर, सिर तथा गर्दन को सीधी रखेंगे, तो रीढ़ भी सीधी रहेगी। कुण्डलिनी धीरे-धीरे सुषुम्ना के द्वारा ऊपर उठती है। ऐसा करने से आपको नींद भी नहीं आयेगी।
यदि आप प्रत्याहार में अच्छी तरह स्थापित हैं, यदि आपकी इन्द्रियाँ आपके पूर्ण नियन्त्रण में हैं, तो आप एक बड़े शहर के भीतर भी पूर्ण एकान्त और शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। यदि इन्द्रियाँ उपद्रवी हैं, यदि आपके पास इन्द्रियों को खींचने की शक्ति नहीं है, तो आपको एकान्त गुफा में भी मन की शान्ति नहीं मिल सकेगी। एक कामुक व्यक्ति जिसने अपने मन और इन्द्रियों को नियन्त्रित नहीं किया हो, वह चाहे हिमालय की एकान्त गुफा में निवास कर रहा हो, तो भी वह हवाई किले बनाता रहेगा।
नासिकाग्र पर स्थिर दृष्टि से देखें तथा मन को आत्मा पर ही लगाये रखें। गीता के ५ वें अध्याय के २५ वें श्लोक में भगवान् कृष्ण कहते हैं—“मन को आत्मा में लीन करके अन्य किसी के बारे में विचार नहीं करना चाहिए।” “अन्य दृष्टि है—-भ्रूमध्य-दृष्टि अथवा दोनों भौंहों के मध्य दृष्टि।” यह गीता (अध्याय ५, श्लोक २७) में वर्णित है। इसमें आप नेत्र बन्द रख कर दृष्टि को आज्ञा चक्र पर स्थिर रखें। यदि आप इसका अभ्यास आँखें खुली रख कर करेंगे, तो सिरदर्द भी हो सकता है। बाहरी कण आँखों में गिर सकते हैं। मन का विचलन भी हो सकता है। आँखों पर तनाव न डालें। सहजता से अभ्यास करें। जब आप नासिकाग्र पर धारणा करेंगे, तो आप दिव्य गन्ध का अनुभव करेंगे। जब आप आज्ञा चक्र पर धारणा करेंगे, तो आप दिव्य ज्योति का अनुभव करेंगे। ये अनुभव आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको आध्यात्मिक पथ में धक्का देने के लिए तथा आपको अलौकिक ईश्वरीय शक्तियों के अस्तित्व हेतु सहमत करने के लिए हैं। अभी अपनी साधना को बन्द न करें। योगी गण अथवा भक्त जो भगवान् शिव का ध्यान करते हैं, वे आज्ञा चक्र पर धारणा करते हैं। आप उस दृष्टि का चुनाव कर सकते हैं, जो आपको अधिक अनुकूल लगे।
मन की सभी किरणें एकत्र करके मन को एकाग्र कीजिए। मन को सभी विषय-वस्तुओं से बार-बार वापस खींच कर इसे अपने लक्ष्य अथवा ध्यान के केन्द्र की ओर केन्द्रित कीजिए। धीरे-धीरे आपको मन की एकाग्रता प्राप्त होगी। आपको धैर्यवान् और अध्यवसायी होना चाहिए। आपको अपने अभ्यास में बड़ा ही नियमित होना चाहिए। तभी आप आगे बढ़ेंगे। नियमितता सर्वाधिक आवश्यक है।
आपको नित्य अन्तरावलोकन, आत्म-विश्लेषण तथा आत्म-परीक्षण के द्वारा मन के मार्गों तथा आदतों को जानना चाहिए। आपको मन के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। तब आपके लिए मन का भटकाव रोकना आसान है। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, जब आप सांसारिक विचारों को भूलने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, तो सभी प्रकार के सांसारिक विचार, असम्बद्ध और बेकार विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं। और आपके मन में बाधा डालते हैं। आप स्तब्ध रह जाते हैं। पुराने विचार जो आपको कुछ वर्ष पूर्व अच्छे लगते थे तथा भूतकाल के आनन्द की पुरानी यादें उमड़ उठती हैं और ये मन को विभिन्न दिशाओं में भटकने के लिए जोर डालती हैं। आप पायेंगे कि अवचेतन मन में स्थित स्मृतियों और विचारों के बृहत् कोष का ऊपरी दरवाजा खुल गया है और विचार एक निरन्तर प्रवाह की भाँति बाहर निकल रहे हैं। आप जितना अधिक उनको रोकने का प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक वे दुगनी शक्ति और बल से उमड़ेंगे।
आपको निराश नहीं होना है। कोई निराशा नहीं। कभी निराश न हों। नियमित तथा निरन्तर ध्यान से आप अवचेतन मस्तिष्क को शुद्ध कर सकेंगे तथा विचारों और स्मृतियों को नियन्त्रित कर सकेंगे। ध्यान की अग्नि सभी विचारों को दग्ध कर देगी। इस विषय में निश्चिन्त रहें। ध्यान विषैले सांसारिक विचारों को दूर करने के लिए एक अचूक रामबाण औषधि है। इस पर विश्वास रखें।
अन्तरावलोकन के समय आप मन के एक विचार से दूसरे विचार की ओर जाने को स्पष्टतया अनुभव करेंगे। यहाँ पर आपके लिए वह परिवर्तन निहित है, जब आप मन को उचित ढंग से मोड़ सकते हैं तथा विचारों और मानसिक ऊर्जा को दैवी स्रोत में निर्दिष्ट कर सकते है। आप विचारों को पुनः क्रमबद्ध कर सकते हैं। एक नये सात्त्विक आधार पर नया सयोजन बना सकते हैं। आप निरुपयोगी सांसारिक विचारों का उसी प्रकार उन्मूलन कर सकते हैं, जिस प्रकार आप खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। आप अपने मन के दैवी बगीचे- अन्तःकरण में उत्कृष्ट दैवी विचारों को उगा सकते हैं। यह एक अत्यन्त धैर्यपूर्ण कार्य है। यह एक विलक्षण कार्य है। लेकिन आत्मदृढ़ व्यक्ति के लिए, जिस पर भगवान् की कृपा हो तथा जिसका लौह संकल्प हो, उसके लिए यह कुछ नहीं है।
अमर आत्मा पर ध्यान एक विस्फोटक की भाँति कार्य करता है तथा ध्यान अवचेतन मस्तिष्क के सभी विचारों और स्मृतियों को जला डालता है। यदि आपको विचार बहुत अधिक परेशान करते हैं, तो उनको बलपूर्वक न दबायें। एक बाइस्कोप की भाँति शान्त साक्षी बनें। वे धीरे-धीरे शान्त हो जायेंगे। फिर उनको नियमित शान्त ध्यान के द्वारा जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करें।
ध्यान का अभ्यास निरन्तर किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही मात्र कोई आत्म-साक्षात्कार निश्चित और शीघ्र प्राप्त कर सकेगा। वह जो आवेश में आ कर ध्यान का अभ्यास प्रारम्भ करता है और नित्य मात्र कुछ देर तक ही अभ्यास करता है, वह योग में किसी प्रकार के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेगा।
कोई भी अपने आत्म-संयम का परीक्षण एक एकान्त जंगल में कैसे कर सकता है, जहाँ पर किसी प्रकार के प्रलोभन ही नहीं हैं। गुफा के योगाभ्यासी को भली प्रकार विकास हो जाने पर आत्म-संयम का परीक्षण समतल स्थानों में जा कर करना चाहिए। लेकिन उसे अपने आत्म-संयम का परीक्षण उस मनुष्य की भाँति जल्दी-जल्दी करने नहीं जाना चाहिए, जो एक पौधे को जल से सींचने के बाद बार-बार उखाड़ कर देखता है कि उसकी जड़ें गहरी गयी हैं कि नहीं।
आप मन तथा सभी इन्द्रियों पर संयम करने के द्वारा तथा नियमित और निरन्तर ध्यान के द्वारा योग में सफलता प्राप्त करें और निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करें!
६. सर्वोच्च शिखर पर पहुँचें
ज्ञानी निरन्तर ध्यान की तेज धार वाली तलवार के द्वारा अहंकार की ग्रन्थि को काट डालता है। तत्पश्चात् आत्मा का परम ज्ञान अथवा पूर्ण अन्तर्ज्ञान अथवा आत्म-साक्षात्कार होता है। मुक्त योगी को अब किसी प्रकार का सन्देह अथवा भ्रम नहीं होता। कर्म के सभी बन्धन कट जाते हैं। इसलिए सदा ध्यान करते रहें। यह अनन्त आनन्द के प्रदेश को खोलने की चाबी है। प्रारम्भ में यह अरुचिकर तथा थका देने वाला होता है; क्योंकि मन बार-बार अपने लक्ष्य से भाग जाता है, लेकिन थोड़े समय के अभ्यास के पश्चात् यह अपने केन्द्र पर एकाग्र हो जायेगा। आप दैवी आनन्द में लीन हो जायेंगे।
एक अद्भुत् अन्तर्ध्वनि आपका पथ-प्रदर्शन करेगी। प्रिय योगीन्द्र! इसे ध्यान से सुनिए ।
जब आपके सामने ज्ञान का प्रकाश चमके, तो भयभीत न हों। यह प्रचुर आनन्द का एक नवीन अनुभव होगा। वापस न लौटें। ध्यान न छोड़ें। यहाँ न रुकें। आपको अभी और आगे बढ़ना है। यह सत्य की एक झलक मात्र है। यह सम्पूर्ण अनुभव नहीं है। यह सर्वोच्च अनुभव या साक्षात्कार नहीं है। यह आपके लिए नवीन धरातल है। अब इस धरातल पर दृढ़ता से खड़े रहिए। आगे बढ़ने का प्रयास करिए। भूमा, अनन्त अथवा पूर्णता तक पहुँचिए। आप निरन्तर अमृत का पान करेंगे। यह अन्तिम अवस्था है। अब आप स्थायी विश्राम कर सकते हैं। अब आपको और अधिक ध्यान की आवश्यकता नहीं।
एक अँधेरे कमरे में एक बर्तन के भीतर जलता हुआ दीपक रखा है। यदि वह बर्तन टूट जाता है, तो कमरे का अँधेरा अदृश्य हो जाता है और आपको कमरे में सर्वत्र प्रकाश दिखायी देने लगता है। इसी प्रकार यदि आत्मा पर निरन्तर ध्यान के अभ्यास के द्वारा यह शरीर रूपी पात्र टूट जाता है अर्थात् यदि आप अविद्या तथा इसके प्रभाव (देहाध्यास) को नष्ट कर दें तथा शरीर-चेतना से ऊपर उठ जायें, तो आप आत्मा के परम प्रकाश का सर्वत्र अनुभव करेंगे।
जिस प्रकार एक जल से भरे पात्र को यदि समुद्र में रख दिया जाये, तो पात्र के टूटने पर इसका जल समुद्र के जल के साथ एक हो जाता है, इसी प्रकार यदि आत्मा पर ध्यान के द्वारा यदि यह शरीर रूपी पात्र टूट जाता है, तो जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है।
जिस प्रकार एक विद्यार्थी प्रारम्भ में अरुचिकर होने पर भी परीक्षा पास करने पर प्राप्त होने वाले परिणाम के बारे में विचार करके भूगोल अथवा गणित विषय के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आपको भी ध्यान के निरन्तर अभ्यास से प्राप्त होने वाले अगणित लाभ जैसे अमरता, परमानन्द तथा अनन्त आनन्द का विचार करके ध्यान में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए।
एक मनुष्य जिसने बद्रीनारायण में निवास करने वाले स्वामी रामकृष्णानन्द को कभी नहीं देखा है, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने उन्हें वास्तव में देखा है और उनको भली प्रकार जानता है, स्वामी रामकृष्णानन्द के व्यक्तित्व के बारे में सुनता है, तो वह मानसिक रूप से उनका चित्र निर्मित कर लेता है, उसी प्रकार एक साधक को एक सन्त जिसने कि आत्म-साक्षात्कार प्राप्त किया हो, उससे अदृश्य ब्रह्म के बारे में सब-कुछ सुन कर फिर आत्मा पर ध्यान करना चाहिए।
जिस प्रकार एक बत्ती लालटेन में जलती है, उसी प्रकार दैवी ज्योति आपकी हृदय-गुहा में अनन्त काल से जल रही है। अपने नेत्र बन्द कीजिए और स्वयं को दिव्य ज्योति में लीन कर दीजिए। अपनी हृदय गुहा में गहरे गोता लगायें, इस दैवी ज्योति पर ध्यान करें और भगवान् की ज्योति बन जायें।
जब आप एक पुस्तक को पूर्ण रुचि के साथ पढ़ते हैं, तो आप उस व्यक्ति की आवाज नहीं सुन पाते जो आपको आपका नाम ले कर चिल्ला-चिल्ला कर पुकार रहा है। उस समय आप सामने मेज पर रखें फूलदान से पुष्पों की मधुर सुगन्ध को भी नहीं सूँघ पाते। यह मन की एकाग्रता है। इस समय मन एक वस्तु पर दृढ़ता से केन्द्रित है। जब आप भगवान् के बारे में विचार करें, तो आपको इसी प्रकार की गहन एकाग्रता रखनी होगी। मन को सांसारिक विषयों पर एकाग्र करना आसान है; क्योंकि आदत के कारण यह स्वयं ही उनमें रुचि लेता है। विषयी लीकें मस्तिष्क में पहले से ही कटी हुई हैं। आपको धीरे-धीरे नित्य ध्यान के अभ्यास के द्वारा, मन को बार-बार ईश्वर के चित्र पर अथवा अपने भीतर की आत्मा पर लगा कर मन को प्रशिक्षित करना होगा। आपको नित्य ध्यान के अभ्यास के द्वारा मन में नवीन आध्यात्मिक लीकें काटनी होंगी। मन को नित्य ध्यान के अभ्यास के द्वारा अत्यधिक आनन्द का अनुभव होगा, अब वह बाह्य विषयों की ओर नहीं भागेगा।
ध्यान का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास एक-दूसरे पर निर्भर है। यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं. तो आपको धारणा प्राप्त होगी। प्राणायाम ही एकाग्रता प्राप्त होती है। एक हठयोगी प्राणायाम का अभ्यास करता है और मन पर नियन्त्रण करता है। एक राजयोगी ध्यान करता है और इस प्रकार प्राणों को नियन्त्रित से स्वत: करता है। वह ऊपर से नीचे की ओर आता है। दोनों ही अन्त में एक ही धरातल पर मिलते हैं। विभिन्न क्षमताओं, रुचियों तथा स्वभावों के अनुसार भिन्न-भिन्न साधनाएँ हैं।
कुछ को प्रारम्भ में प्राणायाम करना सरल लगता है और कुछ को पहले ध्यान करना अधिक सरल लगता है। इसमें बाद वाले साधक (जो कि पहले ध्यान का अभ्यास करता है) ने प्राणायाम का अभ्यास पूर्व जन्म में किया है। इसलिए वे इस जन्म में योग के अगले अंग ध्यान को लेते हैं।
७. ध्यान में गलतियाँ
तन्द्रा और मनोराज्य के मिश्रण को साधक गलती से गहन ध्यान और समाधि समझ बैठते हैं। मन धारणा में स्थापित और विक्षेप से मुक्त प्रतीत होता है। यह एक गलती है। मन को निकटता से देखें। विचार, प्राणायाम तथा हलके सात्त्विक आहार के द्वारा इन दोनों गहन बाधाओं को दूर करें। विचारशील, सावधान और जागरूक बनें। यदि तन्द्रा आये, तो १० मिनट खड़े रहें, सिर और चेहरे पर शीतल जल के छींटे मारें।
कभी-कभी लोभ की अवस्था एक एकाग्रता की स्थिति को उत्तेजित करती है। आप कहीं और केन्द्रित रहते हैं, पर लक्ष्य पर नहीं। इसे देखें और मन को वापस ले आयें। अनेक लोगों द्वारा गहन निद्रावस्था को समाधि समझ लिया जाता है। समाधि सकारात्मक वास्तविक अवस्था है। यह सम्पूर्ण ज्ञान है। गलतियाँ न करें। ध्यान के समय जब आप समता की शान्त अवस्था में प्रवेश करें, जब आप एक विशेष प्रकार की एकाग्रता — आनन्द का अनुभव करें, तो सोचें कि आप समाधि में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवस्था को भंग न करें। इसे लम्बे समय तक बनाये रखने का प्रयास करें। इस अवस्था को बड़ी ही सावधानी से देखें।
वस्तुओं को उनके उचित प्रकाश में जानें। भ्रमित न हों। आवेगों को भक्ति न समझें। संकीर्तन के समय दैवी भावोन्माद के लिए जोर-जोर से कूदना, भाव समाधि के लिए बहुत अधिक कूदने के कारण भूमि पर बेहोश हो कर गिर पड़ना, दैवी कार्यों तथा कर्मयोग के लिए राजसिक बेचैनी तथा गति, एक तामसिक व्यक्ति को सात्त्विक मनुष्य समझ लेना, गठिया में पीठ में वायु की गति को कुण्डलिनी का ऊर्ध्वारोहण समझना, तन्द्रा और निद्रा को समाधि समझना, मनोराज्य को ध्यान समझ लेना, शारीरिक नग्नता को जीवन्मुक्त अवस्था समझ लेना —यह सब ठीक नहीं है। विवेकी बनना सीखें और ज्ञानी बनें।
तन्द्रा को सविकल्प समाधि और गहन निद्रा को निर्विकल्प समाधि न समझें। तुरीयावस्था अथवा भूमावस्था की महिमा अवर्णनीय है। इसका वैभव अवर्णनीय है। यदि शरीर हलका है, मन निर्मल है, यदि मन में इस समय उत्साह है, तो आप जानें कि आप ध्यान कर रहे हैं। यदि शरीर भारी है, मन सुस्त है, तो जानें कि ध्यान करते समय आप सो रहे थे।
साधकों की सदैव शिकायत रहती है- “मैं पिछले १२ वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ; किन्तु मैंने किसी प्रकार का विकास नहीं किया। मुझे कोई साक्षात्कार नहीं हुआ।" ऐसा क्यों है? क्या कारण है? कारण यह है कि उन्होंने स्वयं को अपनी हृदय-गुहाओं में गहन ध्यान में नहीं लीन किया है। उन्होंने मन को भगवान् के विचारों से सही प्रकार से आत्मसात् नहीं किया है। उन्होंने नियमित क्रमबद्ध साधना नहीं की है। उन्होंने इन्द्रियों को उचित प्रकार से संयमित नहीं किया है। उन्होंने मन की सभी बिखरी हुई किरणों को एकत्रित नहीं किया है। उन्होंने यह आत्म-निर्णय नहीं लिया है कि मैं इसी क्षण आत्म-साक्षात्कार करूँगा। उन्होंने अपना पूर्ण १०० प्रतिशत मन भगवान् को समर्पित नहीं किया है। उन्होंने दैवी चेतना के बढ़ते हुए प्रवाह को तैलधारावत् नहीं बनाये रखा है।
यदि कोई साधक ध्यान में हो और यदि आप उसमें नाड़ी का अनुभव न करें, यहाँ तक कि यदि उसकी श्वास रुक गयी हो, तो भी ऐसा न सोचें कि वह निर्विकल्प समाधि में है। मात्र तभी यह कहा जा सकता है कि उसने वास्तविक समाधि प्राप्त की है, जब कि वह समाधि के पश्चात् परम दैवी ज्ञान के साथ वापस आये। श्वास और नाड़ी विभिन्न अन्य कारणों से भी बन्द हो सकते हैं। यदि कोई भोजन और पानी का त्याग कर दे और थोड़ा ध्यान का अभ्यास करे अथवा वह कुछ देर आसन में स्थिर बैठा रहे, तो भी श्वास और नाड़ी बन्द हो सकती है। साधक के भीतर ध्यान में पूर्ण जागरूकता होनी चाहिए। यदि वह मात्र जड़ अवस्था में रहेगा, तो चाहे वह बाहर ध्वनियों के प्रति असंवेदनशील रहे, तो भी उसे अधिक आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी।
एक बार दो संन्यासी एक अन्य साधु, जो कुछ घण्टों तक श्वास और नाड़ी के बिना बैठा रहता था, के भुलावे में आ गये। उसने उन्हें छला और कुछ पैसे ले के भाग गया। अतः आपको अपने निर्णय में बड़ा सावधान होना चाहिए।
ध्यान के समय स्वयं को जड़ अवस्था में न रहने दें। इस अवस्था को ईश्वर के साथ मिलन न समझे। कुछ घण्टी तक जड़ अवस्था में रहना आवश्यक नहीं है। यह गहन निद्रावस्था की तरह है। यह आपको आध्यात्मिक विकास में सहायता नहीं करेगी। यदि यह समय जप करने, कीर्तन करने, मन्त्र-लेखन करने तथा पवित्र ग्रन्थों का स्वाध्याय करने में लगाया जाये, तो आपका शीघ्र विकास होगा। सतर्क बनें। जागरूकता के साथ देखें। यदि वहाँ सच्चा मिलन अथवा सच्चा गहन ध्यान होगा, तो आपको अवश्य शान्ति, आनन्द और दैवी ज्ञान प्राप्त होगा। आपको सन्देहों, भय, मोह, अहंकार क्रोध, वासना तथा राग-द्वेष से मुक्त होना चाहिए। कुछ सुस्त तथा अल्प अनुभवी साधक इस जड़ अवस्था को निर्विकल्प समाधि समझ लेते हैं। वे मिथ्या तुष्टि प्राप्त करत हैं और अपनी साधना बन्द कर देते हैं।
८. ध्यान हेतु निर्देश
हे साधको! कठोर प्रयत्न करें। सच्चे प्रयत्न करें। नित्य नियमित ध्यान करें। कभी भी ध्यान में एक दिन भी न चूकें। यदि आप एक दिन भी चूक गये, तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा।
अब कोई शब्द नहीं। बहुत हुए तर्क-वितर्क। एक एकान्त कमरे में बैठ जायें। अपने नेत्र बन्द कर लें। गहन शान्त ध्यान करें। उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। उनका नाम ॐ उत्साह, आनन्द और प्रेम के साथ दोहरायें। अपना हृदय प्रेम से भरें। संकल्पों, विचारों और कल्पनाओं को जब वे मन की सतह से उठें, तभी नष्ट कर दें। घूमते हुए मन को वापस खींचें और इसे भगवान् पर लगायें। अब निष्ठा और ध्यान गहन और तीव्र होगा। आँखें न खोलें। अपने स्थान से न हिलें। उनमें लीन हो जायें। हृदय गुहा में गहरे गोते लगायें। देदीप्यमान आत्मा में लीन हो जायें। अमरता का अमृत पीयें। एकान्त का आनन्द लें। मैं यहाँ आपको अकेला छोड़ दूँगा। आनन्द, आनन्द ! शान्ति, शान्ति, शान्ति ! एकान्त !
हे प्रिय राम! अब आप एक दृढ़ आध्यात्मिक किले के भीतर हैं। कोई प्रलोभन आपको प्रभावित नहीं कर सकता। अब आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। आप बिना किसी भय के साधना कर सकते हैं। आपके पास आश्रय हेतु दृढ़ आध्यात्मिक अवलम्बन है। एक बहादुर सिपाही बनें। अपने शत्रु मन को निष्ठुरतापूर्वक मार डालें। शान्ति, समदृष्टि एवं सन्तोष का आध्यात्मिक बाना धारण करें। ब्रह्म-तेज से आपका मुख-मण्डल देदीप्यमान हो रहा है। सर्व कृपालु भगवान् ने आपको सभी प्रकार के आराम और उत्तम स्वास्थ्य तथा पथ-प्रदर्शन हेतु एक गुरु प्रदान किया है। अब और अधिक आपको क्या चाहिए? बढ़ें। विकास करें। सत्य का साक्षात्कार करें तथा इसकी सर्वत्र घोषणा करें।
अपने विचारों को बार-बार स्पष्ट करें। स्पष्टतया सोचें। गहन धारणा और सही सोच रखें। एकान्त में अन्तरावलोकन करें। उच्च स्तर तक अपने विचारों को शुद्ध करें। विचारों को रोकें। उबलते मन को शान्त करें। जिस प्रकार एक शल्य-चिकित्सा के क्लीनिक में सहयोगी चिकित्सक मात्र एक ही रोगी को अस्पताल के आपरेशन के कमरे में भीतर जाने देते हैं, उसी प्रकार आपको मन के भीतर मात्र एक ही विचार की तरंग को उठने देना है और उसे शान्ति से बैठ जाने देना है। उसके बाद ही अन्य किसी विचार को प्रवेश करने देना है। सभी असम्बद्ध विचार जो हाथ में लिये गये विषय से सम्बन्धित नहीं हैं, उन्हें भगा दें। दीर्घ अभ्यास के द्वारा विचारों के ऊपर कुशलतापूर्वक नियन्त्रण ध्यान में महान् सहायक है।
प्रत्येक विचार को ध्यान से देखें। मन से सभी बेकार विचारों को बाहर कर दें। आपके जीवन का आपके ध्यान के साथ मेल होना चाहिए। आप अपने काम के साथ भी ध्यान को बनाये रखें। बुरे विचारों के बारे में निरन्तर विचार करके उनको नवीन शक्ति न प्रदान करें। उन्हें रोकें। उनके स्थान पर श्रेष्ठ विचार प्रतिस्थापित करें। विचारों के ऊपर नियन्त्रण अचूक औषधि है। आपको एक भी विचार को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।
मन को शान्त करें। विचारों को शान्त करें। मन की बाहर जाने वाली वृत्तियों अथवा ऊर्जाओं को रोकें। भ्रमण करते हुए विचारों को एकत्रित करें।
अपने मस्तिष्क में अनावश्यक सूचनाएँ न एकत्र करें। मन को मन रहित करना सीखें। जो-कुछ आपने सीखा है, उसे भूल जायें। यह अब आपके लिए बेकार है। ऐसा करने पर ही आप ध्यान में मन को दैवी विचारों से आपूरित कर सकेंगे। आप अब नवीन मानसिक शक्ति प्राप्त करेंगे।
एक स्वर्णकार १३ कैरेट स्वर्ण को घरिया में रख कर तेजाब मिश्रित करके तथा कई बार जला कर १५ कैरेट शुद्ध स्वर्ण में बदलता है, उसी प्रकार आपको अपने विषयी मन को धारणा एवं अपने गुरु के शब्दों तथा उपनिषदों के वाक्यों पर मनन अथवा ध्यान, जप अथवा भगवान् के नाम के मानसिक जप के द्वारा शुद्ध करना होगा।
सकारात्मक सदैव नकारात्मक पर विजयी होता है। सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार को भगा देता है। साहस भय को भगा देता है। प्रेम घृणा को नष्ट कर देता है। एकता पृथकता को मिटा देती है। उदारता ईर्ष्या को नष्ट कर देती है। दानशीलता दुःख तथा लोभ को नष्ट कर देती है। स्वयं को सदा सकारात्मक रखें। आपका ध्यान अद्भुत होगा।
मौन रहें। स्वयं को जानें। मन को उनमें विलीन कर दें। सत्य पूर्ण शुद्ध और सरल है । एकान्त और प्रबल ध्यान भगवत्-साक्षात्कार हेतु दो पूर्वापेक्षाएँ है। नकारात्मक विचारों को खदेड़ दें। सदा सकारात्मक बनें। सकारात्मक सदैव नकारात्मक पर विजयी होता है। जब आप सकारात्मक होंगे, तो आप अच्छी तरह ध्यान कर सकेंगे।
जो भी आपका उत्थान करे, उसे आप अपने लाभ के लिए ले सकते हैं। मन का उत्थान करें और अपना लम्बा ध्यान पुनः करने लगें।
यदि आपकी साधना में विघ्न आये, तो उस कमी की पूर्ति सन्ध्या अथवा रात्रि को अथवा अगली सुबह करें। ध्यान ही एकमात्र आपके लिए बहुमूल्य वस्तु है। योग में सफलता तभी सम्भव है, जब साधक गहन और निरन्तर ध्यान का अभ्यास करे। उसे सदैव आत्म-संयम का अभ्यास करना चाहिए; क्योंकि इन्द्रियाँ अचानक उपद्रवी हो जाती हैं। यही कारण है कि भगवान् कृष्ण गीता में कहते हैं—“हे कुन्तीपुत्र! ज्ञानी मनुष्य चाहे वह कितना ही कठोर प्रयत्न कर रहा हो, तो भी उसकी उत्तेजित इन्द्रियाँ उसके मन को खींच ले जाती है। जिस प्रकार उमड़ती हुई लहरें जहाज को जल पर से खींच ले जाती हैं, उसी प्रकार उपद्रवी इन्द्रियाँ उसकी बुद्धि को खींच ले जाती है।"
मन सदा परिवर्तनशील और भ्रमणशील है। मन की भटकने की आदत अनेक प्रकार से प्रकट होती है। आपको मन की इस भटकने की आदत को रोकने के लिए सदा सावधान रहना होगा। एक गृहस्थ का मन सदा सिनेमा थियेटर, सर्कस आदि में भटकता रहता है। किसी साधु का मन वाराणसी, वृन्दावन, नासिक आदि में भटकेगा। अनेक साधु साधना के समय कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकते। मन की भटकने की आदत को एक स्थान, एक प्रकार की साधना, एक गुरु तथा एक प्रकार के योग पर टिके रह कर नियन्त्रित किया जाना चाहिए। घूमते हुए पत्थर पर कोई जमाव नहीं होता। जब आप पढ़ने के लिए कोई पुस्तक उठायें, तो अन्य कोई पुस्तक हाथ में लेने से पूर्व इसे पूरी पढ़ें। जब आप कोई भी काम हाथ में लें, तो अपना सम्पूर्ण हृदय और एकाग्रता इसमें लगायें और कोई अन्य काम हाथ में लेने से पूर्व इसे समाप्त कर दें। एक बार में एक ही कार्य।
वे लोग जिन्होंने किसी प्रकार का योग-संयम अथवा इन्द्रियों, वृत्तियों अथवा अशुद्धियों पर नियन्त्रण का अभ्यास नहीं किया है, उन्हें धारणा अथवा ध्यान के अभ्यास में कठिनाई होती है। उनका मन घड़ी के पेंडुलम की तरह दोलायमान होता रहता है। उनके मन एक जंगली बैल या बन्दर की भाँति सदा घूमते रहते हैं।
किसी भी जीवित प्राणी को लोभ, स्वार्थ, चिड़चिड़ाहट तथा झुंझलाहट के कारण कष्ट न दें। क्रोध या बुरी इच्छा को त्याग दें। झगड़े, गर्म बहस आदि की भावना त्याग दें। तर्क न करें। यदि आप किसी के साथ झगड़ा करेंगे अथवा किसी से बहस करेंगे, तो आप ३-४ दिनों तक ध्यान न कर सकेंगे। आपके मन का सन्तुलन बिगड़ जायेगा। निरर्थक गलियों से अत्यधिक ऊर्जा व्यर्थ बह जायेगी। खून गर्म हो जायेगा। नाड़ियों चूर-चूर हो जायेंगी। आपको सदैव मन को शान्त रखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान मात्र शान्त मन में ही हो सकता है। एक शान्त मन आपके लिए बहुमूल्य वस्तु है।
साधकों को संवेदनशील होना चाहिए तथा शरीर और नाड़ियों को पूर्णतया नियन्त्रण में रखना चाहिए। संवेदनशीलता जितनी अधिक होगी, काम उतना ही कठिन होगा। एक सामान्य आदमी के बिना सुने ही अनेक आवाजें चली जाती है; लेकिन ये उस व्यक्ति को कष्ट दे सकती हैं जो अत्यधिक संवेदनशील है।
अपने विचारों को केन्द्रित करें और उसके द्वारा आत्मा की अन्तर्शक्ति का विकास करें। विचारों का केन्द्रीकरण मन की बाहर जाने वाली आदत को रोकेगा तथा मन की शक्तियों का विकास करेगा। मन के केन्द्रीकरण का अर्थ है आपकी ऊर्जा का केन्द्रीकरण ।
ऊर्जा बेकार की बातों और गपशप में, योजना बनाने तथा अनावश्यक चिन्ता में व्यर्थ हो जाती है। इन तीनों दोषों से मुक्ति पा कर ऊर्जा का संरक्षण करें और इसका सदुपयोग ईश्वर पर ध्यान में करें। तब आप अद्भुत ध्यान कर सकेंगे। यदि आप लोक-कल्याण हेतु किसी प्रकार का सांसारिक कार्य करना चाहें, तो आप निरर्थक लीकों द्वारा बह जाने वाली ऊर्जा के संरक्षण द्वारा आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं।
जिस प्रकार एक मनुष्य जो मूर्खतापूर्वक दो खरगोशों के पीछे भागता है, वह उन दोनों में से किसी को भी नहीं पकड़ पाता। उसी प्रकार वह ध्यानकर्ता जो दो विरोधी विचारों के पीछे भागता है, वह उन दोनों विचारों में से किसी में भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। यदि वह पहले दस मिनट तक दैवी विचार रखता है तथा अगले १० मिनट तक सांसारिक विरोधी विचार रखता है, तो वह दैवी चेतना प्राप्त करने में सफल नहीं होगा। आपको एक ही खरगोश के पीछे बलपूर्वक तथा एकाग्र मन के साथ भागना है। आप निश्चित ही इसे पकड़ लेंगे। आपको सदा दैवी विचार रखना चाहिए। तब आप निश्चय ही शीघ्र भगवद्-साक्षात्कार कर सकेंगे।
वह जो बुरे स्वभाव अथवा मन के विकारों का उन्मूलन किये बिना ऐसा कहता है। तथा कल्पना करता है कि मैं गहन ध्यान का नित्य अभ्यास करूँगा, वह सर्वप्रथम स्वयं को भ्रमित करता है, फिर दूसरों को। वह निश्चय ही प्रथम श्रेणी का पाखण्डी है।
यदि आप ध्यान में स्वयं पर जोर डालेंगे तथा अपनी क्षमता से परे जायेंगे, तो आलस्य तथा अकर्मण्य प्रकृति प्रकट होगी। शम, दम, उपरति तथा प्रत्याहार के अभ्यास से प्रेरित मन की शान्तता के कारण ध्यान स्वाभाविक रूप से आयेगा। आत्मा अथवा ऊर्जा के स्रोत का विचार भी ऊर्जा, शक्ति तथा बल के दोहन हेतु एक अच्छी विधि है।
कम बोलने, मौन के पालन, क्रोध पर नियन्त्रण, ब्रह्मचर्य के पालन, प्राणायाम के अभ्यास तथा असम्बद्ध तथा अनावश्यक विचारों पर नियन्त्रण कर ऊर्जा का संरक्षण करें। आपके भीतर उपर्युक्त अभ्यास के लिए प्रचुर ऊर्जा होनी चाहिए। तब आप स्वर्ग तथा पृथ्वी में विचरण कर सकते हैं।
सभी इन्द्रिय-विषयों को निर्दयतापूर्वक त्याग दें। वे दर्द के गर्भ हैं। मन के सन्तुलन का धीरे-धीरे विकास करें। इन्द्रियों को वशीभूत करें। वासना, क्रोध तथा लोभ का उन्मूलन करें। ध्यान करें तथा अविनाशी आत्मा का दर्शन करें। आत्मा में दृढ़तापूर्वक विश्राम करें। अब आपको कोई चीज आहत नहीं कर सकती। आप अजेय बन गये हैं।
कामुक पुरुष
एक कामुक पुरुष क्या करता है? वह एक ही निन्दनीय कार्य बार-बार करता है और जितनी अधिक-से-अधिक बार अपने पेट को भर सकता है, भरता है। एक आत्म-साक्षात्कार की ज्वलन्त आकांक्षा वाला साधक क्या करता है? वह थोड़ा दूध लेता है और सारे दिन एवं रात ध्यान करता है और आत्मा के अमर आनन्द का उपभोग करता है। दोनों ही अपने तरीके से व्यस्त रहते हैं। पहले वाला जन्म और मृत्यु के चक्र में फँसता है तथा बाद वाला अमरता प्राप्त करता है। आपको इसे सदा दैवी ध्यान में लगाये रखना चाहिए। यदि आप अपने प्रयत्न ढीले कर देंगे, तो बुरे विचार तत्काल प्रवेश करेंगे। निरन्तर अभ्यास से ही मात्र आप मन को सरलता से नियन्त्रित कर सकते हैं।
वैराग्य आवश्यक है
यदि आप योग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सभी सांसारिक सुखों को त्यागना होगा तथा तप और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होगा। तप और ब्रह्मचर्य धारणा और समाधि की प्राप्ति में सहायता करेंगे।
जब आप अग्नि जलाना चाहते हैं, तो आप थोड़ी घास, कागज के टुकड़ों तथा लकड़ी के छोटे टुकड़ों का ढेर लगाते हैं। यदि अग्नि शीघ्र जलानी है, तो आपको इसे मुख से अथवा फुंकनी से फूँक कर बार-बार जलाने का प्रयत्न करना होगा। कुछ समय बाद यह छोटी ज्वाला बन जायेगी। आप इसे बड़े ही प्रयास के द्वारा ही जला पायेंगे। इसी प्रकार ध्यान के प्रारम्भ में नवाभ्यासी ध्यान से पुराने गर्तों में गिरेगा। उसे अपने मन को बार-बार उठाना होगा तथा लक्ष्य पर केन्द्रित करना होगा। जब ध्यान गहन तथा स्थिर होगा, तब वह भगवान् में स्वयं ही स्थापित हो जायेगा और तब ध्यान सहज बन जायेगा। यह आदत बन जायेगा। ध्यान की अग्नि को जलाने के लिए तीव्र वैराग्य तथा प्रबल धारणा की फुंकनी का प्रयोग करें।
जागरूकता
अनेक वर्षों की आध्यात्मिक साधना हो अथवा जब आप प्रगति कर रहे हों और जब आप आध्यात्मिक पथ में स्थिर हों, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। कभी-कभी आप यदि ध्यान में ढीले पड़ेंगे, तो नीचे भी गिर सकते हैं। प्रतिक्रिया भीतर होगी। कुछ लोग १५ वर्षों तक ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो भी उनकी सच्ची प्रगति नहीं हो पाती है। यह उत्सुकता, वैराग्य एवं मोक्ष की प्रबल आकांक्षा की कमी के कारण है।
यदि साधक की छोटी-छोटी चीजों से आहत होने की प्रकृति है, तो वह ध्यान में कोई प्रगति नहीं कर सकता है।
उसे मिलनसार स्नेही प्रकृति तथा सौजन्यता का अर्जन करना चाहिए। तभी यह बुरी आदत नष्ट होगी। कुछ साधक यदि उनकी बुरी आदतों एवं दोषों के विषय में उन्हें बताया जाये, तो वे सरलता से आहत हो जाते हैं। वे विद्रोही हो जाते हैं और उस आदमी से झगड़ा करने लगते हैं जिसने उनके दोषों को बताया है। वे सोचते हैं कि वह व्यक्ति ईर्ष्या अथवा घृणा के कारण झूठ-मूठ की बातें कर रहा है। यह बुरा है। अन्य लोग हमारे दोष सरलता से ढूँढ़ सकते हैं। एक मनुष्य जो अपना अन्तरावलोकन नहीं करता है, जिसका मन बहिर्गामी प्रवृत्तियों वाला है, वह अपने दोष नहीं ढूँढ सकता। आत्माभिमान आवरण की भाँति कार्य करता है और उसकी मानसिक दृष्टि को अन्धा बना देता है। यदि एक साधक आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अन्यों द्वारा बताये गये. अपने दोषों को स्वीकार करना होगा। उसे उनके उन्मूलन हेतु अपनी ओर से अच्छा प्रयत्न करना चाहिए तथा दोष बताने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। तभी मात्र वह आध्यात्मिकता में विकास कर सकेगा।
एक पेटू या विषयी, एक आलसी मनुष्य ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। वह जिसने अपनी जिह्वा तथा अन्य अंगों पर नियन्त्रण किया है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, जो आहार और शयन में संयमित है, जिसने स्वार्थ, वासना, क्रोध और लोभ को नष्ट कर दिया है, वह ध्यान का अभ्यास कर सकता है तथा समाधि में सफलता प्राप्त का सकता है।
विक्षेप ध्यान में महान् बाधा है। मूर्ति उपासना, प्राणायाम, त्राटक, दीर्घ प्रणव का उच्चारण, मनन, विचार तथा प्रार्थना इस भयंकर बाधा को दूर कर सकते हैं। विक्षेप मन का विचलन है। कामनाओं को नष्ट कर दें। योजनाएँ बनाना छोड़ दें। सभी व्यवहार तथा प्रवृत्तियों को कुछ समय के लिए बन्द कर दें।
विपरीत भावना
विपरीत भावना (गलत धारणा कि आत्मा शरीर है और संसार ठोस सच्चाई है) तथा संशय भावना आप पर विजय पा लेती हैं। जिस प्रकार जल खेत में से चूहे के बिल में बह जाता है, उसी प्रकार विषयों के प्रति राग, छुपी हुई सूक्ष्म कामनाओं तथा गुप्त प्रभावों के कारण ऊर्जा गलत लीकों में व्यर्थ बह जाती है। दबी हुई कामनाएँ भी प्रकट होंगी और आपको परेशान करेंगी। आप उन कामनाओं के अनजाने ही शिकार बन जायेंगे।
प्रतिक्रिया
जब आप किसी ऐसे कमरे की सफाई करते हैं जो कि ६ माह से बन्द है, तो कमरे के कोनों में से अनेक प्रकार की धूल बाहर आती है। इसी प्रकार ध्यान के समय योग के दबाव से तथा भगवान् की कृपा से अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ मन की सतह पर तैरती हैं। साहस के साथ एक-एक करके अनुकूल विधियों एवं विपरीत गुणों के द्वारा धैर्य तथा कठोर प्रयत्नों से उनका उन्मूलन करें। जब आप बुरे व पुराने संस्कारों को दबाने की चेष्टा करेंगे, तो वे आपसे बदला लेंगे। भयभीत न हों। वे कुछ समय बाद अपनी शक्ति खो बैठेंगे। जिस प्रकार आप हाथी या शेर को प्रशिक्षण देते हैं, उसी प्रकार आपको मन को प्रशिक्षित करना होगा। बुरे विचारों में लिप्त न हों। ये मन के लिए भोजन की भाँति कार्य करते हैं। मन को अन्तर्मुखी बनायें। उत्तम, गुणवान् तथा श्रेष्ठ विचारों को स्थापित करें। मन को सद्गुणों एवं उत्कृष्ट विचारों से पोषित करें। पुराने कुसंस्कार धीरे-धीरे तनु हो जायेंगे तथा अन्त में नष्ट हो जायेंगे।
अप्रशिक्षित साधक सामान्यतया अपनी स्वयं की कल्पनाओं एवं भावनाओं को गलती से अन्तर की आवाज या आदेश (दैवी आदेश) समझ बैठते हैं। यह अत्यन्त गलत है। कभी-कभी सुन्दर रूप का दृश्य मन को सुख देता है। आखिरकार मन सुख चाहता है। यदि मन को ध्यान के अभ्यास द्वारा निर्गुण ब्रह्म अथवा आत्मा (जो सबके हृदय में बैठा है) के आनन्द का स्वाद लेने या उपभोग करने हेतु प्रशिक्षित किया जाये, तो यह बाहरी सुन्दर रूपों की ओर नहीं भागेगा।
यदि आप अपने इष्टदेवता के चित्र को बन्द आँखों से देख पाने में सक्षम नहीं हैं, यदि आप अपने इष्टदेवता पर अपने मन को एकाग्र करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने द्वारा दोहराये जा रहे मन्त्र की ध्वनि सुनने का अथवा मन्त्र के शब्दों को क्रमवार सोचने का प्रयास कर सकते हैं। यह मन के भटकने को रोकेगा। यह सब विक्षेप के कारण है। कुसंस्कारों की प्रतिक्रिया के कारण विक्षेप अथवा मन के भटकाव रूपी रोग को दूर करने हेतु एकान्त से अधिक चमत्कारिक गोली कोई और नहीं है।
मान लें कि मन ध्यान के समय १ घण्टे में ४० बार बाहर की ओर भागता है। यदि आप इस भटकाव को घटा कर ३८ बार कर लेते हैं, तो यह निश्चय ही महान् विकास है। आपने मन के ऊपर कुछ तो नियन्त्रण पाया। मन के घुमक्कड़पने को रोकने के लिए लम्बे समय तक कठोर प्रयास की आवश्यकता है। विक्षेप अत्यधिक शक्तिशाली है, लेकिन सत्त्व विक्षेप की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अपने सत्त्व को बढ़ायें। आप मन के इस दोलन पर सरलता से नियन्त्रण पा लें।
९. ध्यान हेतु बीस निर्देश
१. एक अलग ध्यान का कमरा रखें। उसे सदैव ताला बन्द करके रखें। कभी भी किसी को भी ध्यान के
कमरे में प्रवेश न करने दें। इसमें अगरबत्ती जलायें। इस कमरे में प्रवेश के पूर्व अपने पैर धोयें।
२. एक शान्त स्थान अथवा कमरे में विश्राम करें, जहाँ आपको भय न हो। ऐसा इसलिए कि आपका मन
सुरक्षित अनुभव करे और विश्राम करे। वास्तव में सदैव आदर्श स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। जिस
मामले में आप जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हों, करें। आपको भगवान् अथवा ब्रह्म के साथ सम्पर्क के समय में अकेला होना चाहिए।
३. प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त में जागें और ४ से ६ बजे तक ध्यान करें। एक अन्य बैठक ७ से ८ बजे शाम को
करें।
४. अपने इष्टदेवता का चित्र तथा कुछ धार्मिक पुस्तकें गीता, उपनिषद्, योगवासिष्ठ, भागवत आदि
कमरे में रखें। अपना आसन चित्र के सामने बिछायें।
५. पद्म, सिद्ध, सुख अथवा स्वस्तिक आसन में बैठें। सिर, गर्दन एवं धड़ एकदम एक सीध में रखें। आगे
अथवा पीछे न झुकें।
६. अपनी आँखें बन्द करें और सहजता से मन को त्रिकुटी (दोनों भौहों के मध्य स्थान) पर केन्द्रित करें।
उँगलियों को बाँधे रखें।
७. कभी मन से संघर्ष न करें। धारणा में किसी प्रकार का हिंसात्मक प्रयत्न न करें। सभी मांसपेशियों तथा
नाड़ियों को ढीला करें। मस्तिष्क को विश्राम दें। अपने इष्टदेवता के बारे में सहजतापूर्वक चिन्तन करें। धीरे-धीरे अपने गुरु मन्त्र का भाव तथा अर्थ सहित जप करें। उमड़ते मन को स्थिर करें। विचारों को शान्त करें।
८. मन के नियन्त्रण में कोई हिंसात्मक प्रयत्न न करें, बल्कि इसे थोड़ा दौड़ने दें और इसके प्रयत्नों को
समाप्त करें। यह अवसर का लाभ लेगा तथा पहले-पहल जब तक कि यह धीरे-धीरे धीमा न पड़ जाये, एक बन्दर की तरह तब तक कूदेगा तथा फिर यह आपके आदेशों के लिए आपकी ओर देखेगा। मन को पालतू बनाने में कुछ समय लगेगा। लेकिन प्रत्येक बार आपको प्रयत्न करना है। थोड़े समय बाद यह आपके पास आयेगा।
९. विचारों की एक पृष्ठभूमि रखें, चाहे आपके इष्ट की मूर्ति मन्त्र के साथ की एक स्थूल पृष्ठभूमि अथवा
यदि आप ज्ञानयोग के विद्यार्थी हैं, तो अनन्त के विचार के साथ ॐ की निर्गुण पृष्ठभूमि हो। यह सभी अन्य सांसारिक विचारों को नष्ट कर देगी और आपको लक्ष्य की ओर ले कर जायेगी। जिस क्षण आप इसे सांसारिक गतिविधियों से मुक्त करेंगे, तो आदत के बल पर मन तत्काल इस पृष्ठभूमि में शरण लेगा।
१०. जब मन लक्ष्य से भागे, तो इसे सांसारिक विषयों से पुनः पुनः वापस खींचें और वहाँ केन्द्रित करें। इस
प्रकार का संघर्ष कुछ महीनों तक चलेगा।
११. जब आप प्रारम्भ में भगवान् कृष्ण पर ध्यान करें, तो उनका चित्र अपने सामने रखें। उसे अपलक
स्थिर दृष्टि से देखें। पहले उनके पैरों को देखें, उसके बाद रेशमी पीताम्बर को, उसके बाद उनके गले की माला को, उसके बाद मुख को, उसके बाद कुण्डलों को, मस्तक के हीरे जड़ित मुकुट को, उसके बाद बाजूबन्द कंगनों को, उसके बाद शंख, चक्र, गदा और पद्म को। इसके बाद पुनः यही विधि प्रारम्भ करें। इसे बार-बार आधा घण्टे तक करें। जब आप थकान का अनुभव करें, तो स्थिर दृष्टि से मात्र भगवान् के मुख को देखें। इस अभ्यास को तीन माह तक करें।
१२. उसके बाद अपनी आँखें बन्द करें। मानसिक रूप से चित्र को देखें और मन को विभिन्न भागों पर
घुमायें जैसा कि आपने पूर्व में किया है।
१३. आप भगवान् के गुणों जैसे सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता, पवित्रता, पूर्णता आदि को भी अपने ध्यान में
संयुक्त कर सकते हैं।
१४. यदि बुरे विचार आपके मन में प्रवेश करें, तो उन्हें भगाने में अपनी संकल्प-शक्ति का प्रयोग न करें।
आप मात्र अपनी ऊर्जा गँवायेंगे। आप अपनी संकल्प-शक्ति पर भार डालेंगे। आप स्वयं को थकायेंगे। आप जितना अधिक प्रयत्न करेंगे, बुरे विचार उतनी ही अधिक दुगनी शक्ति से आयेंगे। वे अधिक शीघ्रता से वापस आयेंगे और वे विचार अधिक शक्तिशाली बन जायेंगे। निरपेक्ष बनें। शान्त रहें। वे शीघ्र चले जायेंगे। इनके स्थान पर अच्छे विपरीत विचारों को प्रतिस्थापित (प्रतिपक्ष भावना विधि) करें या ईश्वर के चित्र एवं मन्त्र के बारे में बार-बार बलपूर्वक विचार करें अथवा प्रार्थना करें।
१५. कभी भी ध्यान में एक दिन भी न चूकें। नियमित एवं व्यवस्थित ध्यान करें। सात्त्विक भोजन लें।
फल तथा दूध मानसिक एकाग्रता में सहायता करेंगे। मांस, मछली, अण्डे, सिगरेट और शराब को छोड़ दें।
१६. तन्द्रा को हटाने के लिए चेहरे पर ठण्डे पानी के छींटे मारें। १५ मिनट खड़े रहें। सिर की चोटी को एक
डोरी से छत पर कील से बाँध लें। जैसे ही आपको झपकी आयेगी, यह डोरी आपको खींच लेगी और जगा देगी। यह आपकी माँ की भूमिका हिलाये । १० या २० हल्क कुम्भक प्राणायाम करें। शीर्षासन और मयूरासन करें। रात के निभायेगी। एक स्वचालित झूले पर १० मिनट तक बैठें और स्वयं को आगे-पीछे समय मात्र दूध और फल लें। उपर्युक्त विधियों के द्वारा आप निद्रा पर विजय पा सकेंगे।
१७. अपने साथियों के चुनाव में सावधान रहें। टाकीज जाना छोड़ दें। बातें कम करें। दो घण्टे तक नित्य
मौन रखें। अनावश्यक लोगों के साथ न मिलें। अच्छी प्रेरक धार्मिक पुस्तक पढ़े (यदि आप सकारात्मक अच्छी संगत प्राप्त न कर सकें, तो यह एक नकारात्मक अच्छी संगत है)। सत्संग में जायें। ये सभी ध्यान में सहायक हैं।
१८. अपने शरीर को न हिलायें। चट्टान की तरह इसे दृढ़ रखें और शरीर को बार-बार न खींचें। जैसा आपके
गुरु ने बताया है, वैसा ही मानसिक भाव रखें।
१९. जब मन थक जाये, तो धारणा न करें। थोड़ा विश्राम दें।
२०. जब एक विचार मन को बहुत अधिक आपूरित कर लेता हैं, तो यह वास्तविक भौतिक अथवा मानसिक
अवस्था में रूपान्तरित हो जाता है। इसलिए आप मन को मात्र भगवान् के विचारों अथवा भगवान् से ही आपूरित रखें। आप अत्यन्त शीघ्र निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रयत्न करें, सही प्रकार से प्रयत्न करें।
१०. ध्यान में क्रियाएँ
१. भगवान् ईसामसीह का एक चित्र अपने सामने रखें। अपने प्रिय आसन में बैठे। चित्र पर सहजतापूर्वक
तब तक धारणा करें, जब तक कि आँखों से अश्रु बह कर आपके गालों पर न लुढ़कने लगें। मन को उनके वक्ष, लम्बे बाल, सुन्दर दाढ़ी, गोल आँखों तथा उनके शरीर के विभिन्न अंगों तथा सिर के चारों ओर सुन्दर आध्यात्मिक आभामण्डल आदि पर घुमायें। उनके जीवन, उनके चमत्कारों तथा विभिन्न विशिष्ट शक्तियाँ जो उनके पास थीं, उनके बारे में विचार करें। उसके बाद आँखें बन्द कर लें और चित्र को देखें। बार-बार इसी विधि को दोहरायें।
२. भगवान् हरि का चित्र अपने सामने रखें। अपने ध्यान के आसन में बैठ जायें। तब तक आराम से चित्र
पर धारणा करें, जब तक आपको आँसू न आने लग जायें। मन को उनके पैरों, पीताम्बर, वक्ष पर हीरों का हार, कौस्तुभ मणि, कुण्डल पर, तत्पश्चात् इसे मुख मण्डल, सिर के मुकुट, ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र, बायें ऊपरी हाथ में शख, निचले दाहिने हाथ में गदा तथा बायें नीचे के हाथ में पद्म पर घुमायें। उसके बाद नेत्र बन्द कर लें और चित्र देखने का प्रयास करें। इसी विधि को बार-बार दोहरायें।
३. भगवान् कृष्ण का मुरली हाथ में लिये हुए चित्र रखें। अपने ध्यान के आसन में बैठ जायें और चित्र पर
तब तक सहजता से धारणा करें, जब तक आपके अश्रु न बहने लगे। उनके पैरों में पायल, पीताम्बर, गले में विभिन्न हार तथा कौस्तुभ मणि, सुन्दर रंग-बिरंगे फूलों वाली सुन्दर मालाओं, कर्ण-कुण्डलों, अमूल्य मोतियों से ज मुकुट, घने काले बालों, चमकदार नेत्रों, माथे पर तिलक, उनके सिर के चारों ओर का चुम्बकीय आभा मण्डल, लम्बे हाथ जिनमें बाजूबन्द एवं कंगन हैं तथा वंशी जिसे वे बजाने ही वाले हैं, इन सबको देखें। उसके बाद नेत्र बन्द कर लें और चित्र को देखने का प्रयत्न करें। यही विधि बार-बार दोहरायें।
४. यह नवाभ्यासियों हेतु ध्यान का एक प्रकार है। अपने ध्यान के कमरे में पद्मासन में बैठ जायें। नेत्र
बन्द कर लें। सूर्य के प्रकाश, चन्द्रमा की चाँदनी अथवा सितारों की द्युति पर ध्यान करें।
५. सागर की विशालता तथा इसकी अनन्त प्रकृति पर ध्यान करें। उसके पश्चात् सागर की तुलना अनन्त
ब्रह्म के साथ करें तथा लहरों, झाग और आइस वर्ग की तुलना विभिन्न नाम तथा रूपों से करें। स्वयं को समुद्र के साथ एक करें। मौन बनें। विस्तार करें। विस्तार करें।
६. यह एक अन्य प्रकार का ध्यान है। हिमालय पर ध्यान करें। कल्पना करें कि गंगा का उत्तरकाशी के
पास गंगोत्री के बर्फीले क्षेत्र में से उद्गम हो रहा है। वहाँ से यह ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी से होते हुए गंगासागर के पास बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। हिमालय, गंगा और समुद्र — मात्र इन तीनों के विचार ही आपके मन को अधिग्रहीत करने चाहिए। सबसे पहले अपने मन को गंगोत्री के बर्फीले क्षेत्रों में ले जायें, फिर गंगा के साथ-साथ अन्त में समुद्र को जायें। मन को इस प्रकार १० मिनट के लिए घुमायें।
७. एक जीवित ब्रह्माण्डीय शक्ति है जो इन सब नाम और रूपों में निहित रहती है। इस शक्ति पर जो कि
निराकार है, ध्यान करें। यह निर्गुण, निराकार चेतना परमात्मा के साक्षात्कार में बदल जायेगी।
८. पद्मासन में बैठ जायें। अपनी आँखें बन्द कर लें। मात्र निराकार वायु पर ही स्थिर दृष्टि से देखें। वायु
पर धारणा करें। वायु की सर्वव्यापक प्रकृति पर ध्यान करें। यह अभ्यास जीवन्त, सत्य, निराकार, नाम रहित ब्रह्म के साक्षात्कार की ओर ले कर जायेगा।
९. अपने ध्यान के आसन में बैठें। अपने नेत्र बन्द कर लें। कल्पना करें कि एक परम अनन्त ज्योति सभी
नाम-रूपों के पीछे छिपी है, जो करोड़ों सूर्यो को एक साथ रखने पर होने वाली ज्वाला के बराबर है। यह निर्गुण ध्यान का एक अन्य प्रकार है।
१०. विस्तृत नीले आकाश पर धारणा और ध्यान करें। यह निर्गुण ध्यान का अन्य प्रकार है। इसके अभ्यास
से धारणा की पूर्व की विधियों द्वारा मन का सीमित रूपों के बारे में विचार करना रुक जायेगा। यह धीरे-धीरे शान्ति के समुद्र में विलीन हो जायेगा, क्योंकि यह इसके विषयों से वंचित हो जायेगा। मन सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता जायेगा।
११. अपने सामने ॐ का चित्र रखें। जब तक अश्रु न बहने लगें, तब तक इस चित्र को सहजतापूर्वक एकटक
देखते रहें। जब आप ॐ के बारे में विचार करें, तो नित्यता, अनन्तता, अमरता आदि के विचारों को संयुक्त करें। मधुमक्खियों की गुनगुन की ध्वनि, बुलबुल की मधुर ध्वनि, संगीत के सात सुर तथा सभी ध्वनियाँ मात्र ॐ से ही निकली हैं। ॐ वेदों का सार है। कल्पना करें— ॐ एक धनुष है, मन तीर है तथा ब्रह्म लक्ष्य है। बड़ी ही सावधानी से लक्ष्य को भेदें। जिस प्रकार तीर लक्ष्य के साथ एक बन जाता है, उसी प्रकार आप ब्रह्म के साथ एक बन जायें। ॐ का छोटा नाद सभी पापों को भस्म कर देता है, लम्बा नाद मोक्ष देता है तथा दीर्घकरण सभी सिद्धियाँ प्रदान करता है। वह जो इस एकाक्षर ॐ का उच्चारण करता और इस पर ध्यान करता है, वह जगत् के सभी शास्त्रों पर ध्यान करता है और उच्चारण करता है।
१२. अपने ध्यान के कमरे में पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ कर अपने श्वास का प्रवाह देखें। आप 'सोऽहं'
की ध्वनि सुनेंगे। भीतर लेते समय 'सो' की ध्वनि तथा 'हं' की ध्वनि रेचक के समय। सो का अर्थ है- "मैं वह हूँ।" श्वास आपकी परमात्मा के साथ एकता की ओर संकेत करती है। आप अचेतन रूप से १५ 'सोऽहं प्रति मिनट की दर से नित्य २१६०० 'सोऽहं' का जप करते हैं। 'सोऽहं' के साथ पवित्रता, शान्ति, पूर्णता, प्रेम आदि के विचारों को संयुक्त करें। मन्त्र जप के समय शरीर को विस्मृत कर दें तथा स्वयं को मन्त्र के साथ आत्मा अथवा परमात्मा के साथ पहचानें।
१३. उद्धव ने भगवान् श्री कृष्ण से प्रश्न किया- "हे कमल नयन ! आप पर ध्यान कैसे किया जाये? कृपा
करके मुझे बतायें कि ध्यान की प्रकृति क्या है और ध्यान क्या है ?” इसके लिए भगवान् श्री कृष्ण ने उत्तर दिया – “एक ऐसे आसन पर बैठ जायें जो न ऊँचा हो न नीचा तथा आरामदेह हो, शरीर सीधा हो और अपने हाथों को गोद में रख लें। अपनी दृष्टि को नासिकाग्र पर केन्द्रित करें। दायें नासारन्ध्र को अँगूठे से बन्द करें अर्थात् पहले बायें नासारन्ध्र से श्वास भीतर लें, तत्पश्चात् बायें नासारन्ध्र को अनामिका उँगली तथा कनिष्ठिका उँगली से बन्द कर लें और श्वास को दोनों नासारन्ध्री में रोक कर रखें। इसके बाद अँगूठा उठायें और दायें नासारन्ध्र से श्वास को बाहर निकालें। इसी विधि को विपरीत प्रकार से करें। श्वास को दायें नासारन्ध्र से भरें, तत्पश्चात् दोनों नासारन्ध्रों में श्वास को रोकें और इसके बाद श्वास को बायें नासारन्ध्र से बाहर निकालें। इस प्राणायाम का अभ्यास धीरे-धीरे इन्द्रियों पर संयम के साथ करें और इस प्रकार प्राण के मार्ग को शुद्ध करें।
"एक घण्टी की ध्वनि के साथ ॐ का मूलाधार से ले कर ऊपर तक सर्वत्र विस्तार हो जाता है, ॐ को प्राण (बारह अंगुल ऊँचा) के साधन से हृदय में उठायें जैसे कि यह कमल के डण्ठल का तन्तु हो। वहाँ बिन्दु (ध्वनि का १५वाँ व्यंजन) को इसके साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार शब्द को दस बार दोहराते हुए ॐ के साथ संयुक्त करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास को दिन में तीन बार करना चाहिए। तीन माह के भीतर आप प्राणवायु पर नियन्त्रण प्राप्त कर सकेंगे। जिस प्रकार केले के फूलों की धड़ होती है, उसी प्रकार हृदय-कमल का डण्ठल ऊपर की ओर है और फूल का मुख नीचे की ओर। इसका ध्यान इस प्रकार करें कि इसकी आठों पंखुड़ियाँ खुली हुई है और यह पूर्ण विकसित है। ऐसी कल्पना करें कि बीज कोष के ऊपर सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि एक के बाद स्थित हैं। सर्वप्रथम समस्त अंगों पर ध्यान करो। उसके बाद इन्द्रियों को उनके विषय से वापस खींचो। उसके बाद बुद्धि के साधन के द्वारा एकाग्र मन को पूर्णतः मेरी ओर खींचो। उसके बाद सभी अन्य अंगों को त्याग दो और किसी भी चीज पर न ध्यान करो। मात्र मेरे मुस्कराते चेहरे पर ही धारणा करो। इसके बाद एकाग्र मन को उससे भी खींच लो और इसे आकाश पर केन्द्रित करो। इसे भी त्याग दो और मन को मुझ पर (ब्रह्म की भाँति ) एकाग्र करो और किसी के बारे में बिलकुल विचार न करो। तुम आत्मा में मुझे उसी प्रकार देखो जैसे यह सभी आत्माओं के साथ एक है, जैसे प्रकाश दूसरे प्रकाश के साथ एक हो जाता है। विषयों, ज्ञान तथा कर्म के बारे में भ्रम तब पूर्णतया अदृश्य हो जायेगा।'
यह भागवत पुराण में स्वयं भगवान् कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट ध्यान हेतु अत्यन्त सुन्दर विधि है।
११. ध्यान की अवस्था
सामान्यतया जब आपको स्वप्न रहित अथवा गहन निद्रा आती है, तो आपको में चले जाते हैं, जो लगभग मृत्यु, एक मृत्यु का अनुभव है। लेकिन एक ऐसी भी निद्रा कुछ भी याद नहीं रहता कि आपने स्वप्न में क्या देखा अथवा आप पूर्ण अचेतनावस्था की सम्भाव्यता है जहाँ आप अपने सम्पूर्ण शरीर में एक पूर्ण शान्ति में प्रवेश करते हैं। तथा आपकी चेतना सत्-चित्-आनन्द में विलीन हो जाती है। आप इसे निद्रा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें पूर्ण जाग्रति रहती है। इस अवस्था में आप मात्र कुछ मिनटों तक ही रह सकते हैं। यह आपको कई घण्टों की साधारण निद्रा की अपेक्षा अधिक विश्राम तथा ताजगी प्रदान करती है। इसे आप अवसर से प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए लम्बे प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
जब आपका ध्यान गहन हो जाता है, तो आप सामान्यतया मात्र सूक्ष्म कारण शरीर से कार्य करते हैं। कारण शरीर चेतना आपकी सहज चेतना बन जाती है। भगवान् गौरांग, तुकाराम, तुलसीदास ने स्वयं को कारण शरीर चेतना से एक कर लिया था और सहज कारण शरीर चेतना प्राप्त कर ली थी। भक्त भी ब्रह्म के साथ एक बन जाता है। उसके पास दैवी ऐश्वर्य होते हैं, चाहे उसका शरीर दुर्बल होगा। वह अपनी वैयक्तिकता को बनाये रखता है। एक भँवर सम्पूर्ण जल के साथ एक हो जाता है। यह एक पृथक अस्तित्व भी है। ऐसा ही भक्त के विषय में भी है जिसका उसके कारण शरीर के साथ जीवन है।
आपको ध्यान की ६ अवस्थाओं को पार करना होगा और अन्त में आप पूर्ण निर्विकल्प समाधि अथवा परम चेतनावस्था में प्रवेश करेंगे। रूप दृष्टि तथा प्रतिविम्ब पूर्ण तथा नष्ट हो जायेगा। अब वहाँ न तो ध्यान होगा न ध्येय। ध्यानकर्ता और ध्येय एक बन गये हैं। आपने अब सर्वोच्च ज्ञान, स्थायी तथा परम शान्ति प्राप्त कर ली है। यही अस्तित्व का लक्ष्य है। यह जीवन का परम लक्ष्य है। आप अब एक स्थापित सन्त या ज्ञान-प्राप्त जीवन्मुक्त कहे जायेंगे। आप दुःख, दर्द, भय, सन्देह तथा मोह से पूर्णतया मुक्त होंगे। आप ब्रह्म के साथ एक हो गये हैं। बुलबुला समुद्र बन गया है, सभी भेद और विक्षेप पूर्णतया नष्ट हो गये हैं। आप अनुभव करेंगे — “मैं अमर आत्मा हूँ। सभी वास्तव में ब्रह्म हैं। यहाँ और कुछ नहीं, बस ब्रह्म है।"
ध्यान के प्रारम्भ में विभिन्न रंगों जैसे लाल, सफेद, नीला, हरा तथा हरे रंग आदि का मिश्रित प्रकाश मस्तक में प्रकट होगा। वे तन्मात्रिक प्रकाश हैं। प्रत्येक तत्त्व का अपना रंग है। पृथ्वी तत्त्व का पीला रंग है। जल तत्त्व का श्वेत रंग है। अग्नि का लाल रंग है। वायु का हरा रंग है। आकाश का नीला रंग है। रंगीन प्रकाश उन तत्त्वों के कारण है।
कभी-कभी ध्यान के समय मस्तक के सामने एक बड़ा सूर्य या चन्द्रमा या बिजली की चमक प्रकट होती है। इन पर ध्यान न दें। उन्हें त्याग दें। इन प्रकाशों के स्रोत में गहरे गोते लगायें।
कभी-कभी ध्यान में देवता गण, ऋषि, नित्य सिद्ध प्रकट होंगे। उनका आदर के साथ स्वागत करें। उनको प्रणाम करें। उनसे सलाह लें। वे आपकी सहायता करने तथा आपको प्रोत्साहन देने के लिए प्रकट हुए हैं।
जब मात्र एक ही वृत्ति होगी, तो आपको सविकल्प समाधि प्राप्त होगी। जब यह प्रवृत्ति भी मृत हो जायेगी, तो आप निर्विकल्प समाधि प्राप्त करेंगे।
समाधि में त्रिपुटी (ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय) नष्ट हो जाती है। ध्याता और ध्येय, विचार और विचारक—दोनों एक हो जाते हैं। समाधि में कोई ध्यान नहीं होता। ध्याता तथा ध्यान, ध्येय में विलीन हो जाते हैं। डरपोक लोग इससे व्यर्थ में घबरा जाते हैं। यह कुछ भी नहीं है। ध्यान से मस्तिष्क, नाड़ियों आदि में परिवर्तन आता है। नयी शक्तिशाली कोशिकाएँ पुरानी कोशिकाओं के द्वारा स्थापित की जाती है। वे सत्त्व से परिपूर्ण रहती हैं। सात्त्विक विचार-तरंगों के लिए नयी नाड़ियाँ, नये समूह, नयी गलियाँ मस्तिष्क और मन में निर्मित हो गयी है। इसी कारण मांसपेशियाँ थोड़ा उत्तेजित हो जाती हैं। साहसी और बहादुर बनें। साहस साधकों के लिए महत्त्व गुण एवं योग्यता है। इस सकारात्मक गुण का अर्जन कीजिए।
कुछ दिनों के लिए सम्भवतया आपको कोई भी परिवर्तन न दिखायी दे। आप स्थिरता का अनुभव करें और झुंझलाहट व्यक्त करें। प्रतिदिन प्रातः अभ्यास करते रहें। वर्तमान में आप इसे झुंझलाहट भरा कहेंगे। आपके मन में अनादेशित विचार चमकेगा - "मुझे धैर्यवान् होना चाहिए।" अभी भी आप अपना अभ्यास करते रहें। शीघ्र ही झुंझलाहट की भावना के साथ धैर्य का विचार प्रकट होगा और इसका बाह्य प्राकट्य रुक जायेगा। अभी भी अभ्यास करते रहें। झुंझलाहट अदृश्य हो जायेगी तथा झुंझलाहट के प्रति धैर्य आपका सामान्य व्यवहार बन जायेगा। इस प्रकार आप सान्त्वना, आत्म-संयम, पवित्रता, विनम्रता, परोपकारिता, श्रेष्ठता, उदारता आदि गुणों को विकसित कर सकते हैं।
मात्र एक प्रशिक्षित मन जो शरीर को नियन्त्रित कर सकता है, वह जिज्ञासा और निरन्तर ध्यान कर सकता है। जब तक जीवन रहे, कभी भी एक क्षण के लिए भी अपनी खोज तथा ध्यान के विषय (ब्रह्म) की दृष्टि को न भूलें, कभी भी इसे किसी भी लौकिक प्रलोभन से एक क्षण के लिए आच्छादित न होने दें।
पूरक के समय वायु १६ अंगुल बाहर आती है। जब यह मन एकाग्र होता है, तो और इसी प्रकार क्रमशः कम होती जाती है। जब आप गहन ध्यान में होते हैं, तो यह कम और कम होती जाती है। यह पहले १५ होती है, फिर १४, १३, १२, १०, ८ और इसी प्रकार क्रमश: कम होती जाती है । जब आप गहन ध्यान में होते हैं, तो नासारन्ध्रों से श्वास बाहर नहीं आती।
इस समय कभी-कभी फेफड़ों तथा पेट में अत्यन्त हल्की गति होगी। श्वास की प्रकृति से आप किसी साधक की धारणा के स्तर का अनुमान लगा सकते हैं। श्वास को बड़ी ही सावधानीपूर्वक देखें।
जब आप आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए ध्यान तथा कार्यालय का कार्य साथ-साथ करना मुश्किल होगा, क्योंकि मन पर दुगना तनाव पड़ेगा। यह ध्यान के समय भिन्न लीकों और नाड़ियों के भिन्न संस्कारों के साथ कार्य करेगा। इसे असम्बद्ध गतिविधियों के भिन्न प्रकारों के साथ सामंजस्य करने में बड़ी ही कठिनाई का अनुभव होगा। जैसे ही यह ध्यान से नीचे आयेगा, यह अन्धकार में घिर जायेगा। यह भ्रमित और परेशान हो जायेगा। इसे भिन्न-भिन्न लीकों एवं नाड़ियों में कार्य करना होगा। जब आप पुनः ध्यान हेतु बैठेंगे, तो आपके दिन के समय जो नवीन अर्जित संस्कार हैं, उन्हें पोंछने तथा मन की एकाग्रता प्राप्त करने हेतु कठिन संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष के कारण कभी-कभी सिरदर्द होने लगेगा। प्राण (ऊर्जा) जो विभिन्न लीकों एवं नाड़ियों में भीतर घूमता है तथा जो ध्यान के समय सूक्ष्म है, उसे सांसारिक गतिविधियों में नवीन विभिन्न नाड़ियों में सांसारिक गतिविधियों में घूमना पड़ता है। यह काम के समय बहुत स्थूल हो जाता है।
मन ध्यान के समय स्थिर होता है, तो नेत्र गोलक भी स्थिर हो जाते हैं। एक योगी जिसका मन शान्त है, उसकी आँखें स्थिर होंगी। वे तनिक भी नहीं झपकेंगी। नेत्र तेजोमय तथा लाल या शुद्ध श्वेत रंग के होंगे।
शुद्धिकरण की प्रक्रिया से सत्य में गहन अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है। यह ध्यान में आत्मा के ऊपर भगवान् की कृपा के कारण होने वाली क्रिया-विधि है। इस अन्तर्प्रवाहित कृपा से वहाँ मन की ज्योति जगती है, जिसमें भगवान् उनके निर्मल वैभव की किरण भेजते हैं। यह प्रकाश अत्यन्त शक्तिशाली होता है।
जब सुषुम्ना नाड़ी कार्य करती है अर्थात् जब दोनों नासारन्ध्रों से श्वास प्रवाहित होती है, तो ध्यान आनन्दपूर्ण एवं सरल होता है। मन इस समय शान्त रहता है। इस समय सत्त्व में वृद्धि रहती है। जब सुषुम्ना प्रवाहित होना प्रारम्भ हो, उसी क्षण ध्यान हेतु बैठ जायें।
ध्यान के अभ्यास से मन-मस्तिष्क और नाड़ी-तन्त्र में अनेक परिवर्तन होते हैं। नवीन नाड़ी - तरंगें, नये स्पन्दन, नयी गलियाँ, नवीन कोशिकाएँ निर्मित होती हैं, सम्पूर्ण मन एवं नाड़ी-तन्त्र का नवीनीकरण होता है। आप एक नवीन हृदय, नवीन मन, नयी संवेदनाएँ, नयी भावनाएँ, विचार करने के नये तरीके तथा विश्व के प्रति नवीन दृष्टिकोण (जैसे भगवान् प्रकट हो) का विकास करते हैं।
ध्यान के कमरे को ईश्वर के मन्दिर की भाँति समझना चाहिए। कलुषित प्रकृति की बातें कभी उस कमरे नहीं की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार के बुरे विचार जैसे विद्वेष, ईर्ष्या, लोभ आदि को उस कमरे में नहीं लाना चाहिए। वहाँ पर सदैव एक पवित्र तथा मौलिक मन के साथ प्रवेश करना चाहिए। जो हम करते, सोचते तथा बोलते हैं, वे कमरे में अपने संस्कार छोड़ देते हैं। यदि उनसे बचने की कोई सावधानी नहीं रखी गयी, तो वे साधक के मन पर अपना प्रभाव डालेगे तथा साधक का मन दृढ़ तथा हठी रखेंगे एवं उसे समर्पण हेतु अयोग्य बना देंगे। जो शब्द बोले गये, जो विचार पोषित किये गये. तथा जो कार्य किये गये, वे कभी नष्ट नहीं होते। वे सदैव जहाँ पर किये गये है, उस कमरे में जो आकाश है, उसकी सूक्ष्म पर्तों पर तैरते रहते हैं और अनिवार्य रूप से मन को प्रभावित करते हैं। इसके लिए जितना अधिक सम्भव हो, प्रयास किया जाना चाहिए। इस हेतु मात्र कुछ माह तक ही प्रयास करना होगा। जब यह आदत परिवर्तित हो जायेगी, प्रत्येक चीज सही हो जायेगी।
जब मन सात्त्विक है, आप अन्तःप्रेरणा की झलक अथवा द्युति प्राप्त कर सकते हैं। आप कविताओं की रचना करेंगे। आप उपनिषदों के महत्त्व को सुन्दर ढंग से समझ सकेंगे। लेकिन यह नवाभ्यासियों में नहीं प्राप्त होगी। तमोगुण तथा रजोगुण मानसिक कार्यशाला में प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। विकास प्रारम्भ में मेंढक की तरह होता है। यह कभी भी स्थिर और निरन्तर नहीं रहता। आप सोच सकते हैं, आप लगभग लक्ष्य तक पहुँच गये हैं, लेकिन १५ से २० दिनों तक और कुछ नहीं, बस हताशा के अलावा और कुछ अनुभव नहीं करेंगे। यह स्थिति से स्थिति कूदता है, लेकिन निरन्तर विकास नहीं होता। एक स्थिर प्रबल वैराग्य रखें तथा प्रबल संरक्षित साधना करें। कुछ वर्षों तक अपने गुरु के प्रत्यक्ष निर्देशन एवं निकट सम्पर्क में रहें। आपकी स्थिर और निरन्तर प्रगति होगी।
जब आप ध्यान में आनन्द का अनुभव करें, तो कुछ विशिष्ट संवेदना आपको बाधित करेगी और इस बाधा के साथ उत्कृष्ट आनन्द अदृश्य हो जायेगा। ध्यान के समय है। आप रजोगुण के प्रवेश के कारण बाधा का एक विशेष संवेदन अनुभव करते हैं। सभी सत्त्व में वृद्धि होती है, लेकिन रजोगुण सदैव सत्त्व पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता कार्मों को भूल जायें और मन से कहें- "मुझे अब कोई काम नहीं करना। मैंने सब कुछ कर लिया है।” कठोर साधना एवं महान् वैराग्य के द्वारा जब सत्त्व में वृद्धि हो जाती है, तो यह बाधा भी नष्ट हो जायेगी और आपका ध्यान गहन हो जायेगा। आनन्द भी लम्बे समय तक रहेगा।
सिद्ध देव गण तथा अन्य लोगों ने उद्दालक मुनि को घेर लिया। अनेकों अप्सराएँ उनके पास आयीं। देवेन्द्र ने उन्हें अपना देवलोक भेंट करने की इच्छा व्यक्त की। उद्दालक मुनि ने कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। अप्सराओं ने अपनी भावभंगिमाओं से उनको आकृष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा- "आइए देव! विमान में स्थान ग्रहण कीजिए। हम आपको देवलोक ले कर जायेंगे। यहाँ वह वसन्त है जो अमरत्व प्रदान करता है। यहाँ स्वर्ग की अप्सराएँ हैं, जो आपकी सेवा करेंगी। आपकी दुर्लभ तपस्या ने यह सब आपको प्रदान किया है। यहाँ पर चिन्तामणि है।” उद्दालक साहसी थे। उन्होंने सभी प्रलोभनों को विजित कर लिया था और तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। वे विषय-वस्तुओं के अभिलाषी नहीं थे। छह माह पश्चात् मुनि अपनी समाधि से जागे। वे गहन समाधि में एक ही बार में दिनों, माहों तथा वर्षों तक बैठे रहते थे और उसके बाद समाधि से जाग जाते हैं। बालि समाधि में लम्बे समय तक मूर्तिवत् बैठे रहते थे। जनक समाधि में मूर्तिवत् लम्बे समय तक बैठे रहते थे। प्रहलाद निर्विकल्प समाधि में अनेक वर्षों तक मूर्तिवत् बैठे रहते थे।
१२. संयम का अभ्यास
धारणा, ध्यान तथा समाधि— तीनों एक साथ मिल कर संयम का निर्माण करते हैं। एक ही समय पर एक साथ इन तीनों के संयुक्त अभ्यास को संयम नाम दिया गया है। बाह्य विषयों पर संयम के द्वारा योगी को विभिन्न सिद्धियाँ तथा विश्व की तन्मात्राओं आदि का गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है। इन्द्रियों, मन एवं अहंकार आदि पर धारणा से उसे विभिन्न शक्तियाँ और अनुभव प्राप्त होते हैं।
ये तीनों (धारणा, ध्यान तथा समाधि) यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार की अपेक्षा अधिक अन्तरंग हैं। ये तीनों सही योग का निर्माण करते हैं। पाँचों साधन योग के बाह्य साधन हैं। ये तीनों सीधे समाधि लाते हैं। अन्य पाँच शरीर, प्राण तथा इन्द्रियों को शुद्ध करते हैं। इसलिए उपर्युक्त तीनों को अन्तरंग साधना कहते हैं।
संयम पर विजय से मिलन की स्थिति आती है। जैसे संयम दृढ़ और दृढ़तर होता. जाता है, वैसे ही समाधि का ज्ञान और अधिक स्पष्ट होता जाता है। यह संयम के अभ्यास का फल है। तब संयम अत्यन्त स्वाभाविक हो जाता है। तब ज्ञान अन्य किसी चीज की भाँति ज्योतित होता है। संयम योगी के लिए शक्तिशाली अस्त्र है। जिस प्रकार एक तीरन्दाज पहले बड़े विषय पर लक्ष्य करता है और फिर वह सूक्ष्म विषयों को लेता है, इसी प्रकार उसे बहुत अधिक अभ्यास करना होगा तथा सीढ़ी दर सीढ़ी योग पर चढ़ना होगा।
सूर्य पर संयम करने से तीनों लोकों का ज्ञान आयेगा। चन्द्रमा पर संयम से सितारों का लोक ज्ञान आता है। ध्रुव तारे पर संयम से तारों की गति का ज्ञान आता है। हाथियों तथा अन्यों की शक्ति पर संयम से उनकी शक्ति आती है।
अन्यों के संकेतों पर संयम करने से उनके मनों का ज्ञान आता है। कर्ण तथा आकाश के सम्बन्ध पर संयम से दिव्य श्रवण-शक्ति आती है। आकाश तथा शरीर के मध्य सम्बन्ध पर संयम से योगी को रुई-सा हलकापन प्राप्त होता है, वायु में गमन की शक्ति आती है।
संस्कारों (मन के संस्कार) के प्रत्यक्ष दृष्टि से तथा संयम के द्वारा पूर्व-जन्म का ज्ञान आता है। सत्त्व एवं पुरुष (आत्मा) के मध्य सम्बन्ध पर संयम से सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमानता की शक्ति प्राप्त होती है। नाभि चक्र पर संयम से शरीर का ज्ञान आता है।
विशुद्ध चक्र पर संयम के द्वारा भूख-प्यास का उन्मूलन होता है। मस्तक के प्रकाश पर संयम करने पर सिद्धों के दर्शन होते हैं।
१३. ध्यान- प्रश्नोत्तरी
प्रश्न : ब्राह्ममुहूर्त क्या है?
उत्तर : प्रातःकाल ४ बजे से ६ बजे तक के समय को ब्राह्ममुहूर्त कहते हैं।
प्रश्न : ऋषियों ने इसकी प्रशंसा क्यों की है?
उत्तर : क्योंकि यह भगवान् अथवा ब्रह्म पर ध्यान हेतु अनुकूल है, इसलिए इसे ब्राह्ममुहूर्त कहते हैं।
हैं?
प्रश्न : इस विशेष समय पर ध्यान करने से साधकों को क्या विशेष लाभ होते हैं ?
उत्तर: इस विशेष समय पर मन बहुत शान्त और स्वच्छ रहता है। यह सांसारिक विचारों, चिन्ताओं और
व्याकुलताओं से मुक्त रहता है। मन एक कोरे कागज की तरह होता है और तुलनात्मक रूप से सांसारिक संस्कारों से मुक्त रहता है। इस समय सांसारिक विचलनों के मन में प्रवेश करने से पहले इसे बड़ी ही सरलतापूर्वक मोड़ा जा सकता है और वातावरण भी इस विशेष समय में अधिक सत्त्व से आवेशित रहता है। बाहर भी कोई कोलाहल अथवा शोर नहीं रहता है।
प्रश्न: क्या मैं ध्यान प्रारम्भ करने के पूर्व स्नान कर सकता हूँ ?
उत्तर : यदि आप अधिक शक्तिशाली हैं, यदि आप स्वस्थ हैं, यदि मौसम और ऋतु अनुकूल हों, यदि आप
युवावस्था के आरम्भ में हैं, तो ठण्ढे, गुनगुने या गर्म पानी से, जैसी भी आवश्यकता हो, स्नान कर लें। ॐ अच्युताय नमः', 'ॐ गोविन्दाय नमः', 'ॐ अनन्ताय नमः' मन्त्रों से आचमन करें।
प्रश्न: ध्यान अथवा मन को एकाग्र करने हेतु कैसे प्रयास करें?
उत्तर : सर्वप्रथम हरि के चतुर्भज स्वरूप पर एक वर्ष तक धारणा करें। उसके बाद निर्गुण ध्यान या किसी
विचार पर ध्यान करें। आप इन पर भी ध्यान कर सकते हैं। ॐ एकं, अखण्ड, चिदाकाश सर्वभूत अन्तरात्मा - एक अविभाज्य आत्मा, प्राणियों के अन्तर्वासी, आकाश की तरह सर्वव्यापक सूक्ष्म चेतना । "
प्रश्न : मेरी सबसे बड़ी परेशानी मन की एकाग्रता के लिए है। मन ध्यान के समय भागता ही रहता है। इस हेतु
उपाय बताइए?
उत्तर : अपने वैराग्य तथा अभ्यास को दृढ़ कीजिए। पुनः पुनः आपको अपने मन को लक्ष्य पर ले कर आना
होगा। यदि आप इसके ५५ बार भागने के स्थान पर यह संख्या घटा कर ५० बार कर दें, तो भी यह आपके लिए महान् प्राप्ति होगी। मौन आपको बड़ी सहायता करेगा। शीत ऋतु में आप ध्यान हेतु सुबह, दोपहर, शाम तथा रात्रि को बैठ सकते हैं।
प्रश्न: मन के लिए जब यह ध्यान के समय सुस्त हो जाता है, तो मैं प्राणायाम के साथ और क्या कर सकता
हूँ? क्या मैं मन को सुझाव दे सकता हूँ?
उत्तर : जब भी मन सुस्त हो जाये, तो संकल्प करें— "मैं आत्मा हूँ। मैं ज्ञान से पूर्ण हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ॐ
ॐ ॐ।” मन शान्त हो जायेगा तथा आपके ध्यान में केन्द्रित हो जायेगा।
प्रश्न : एक योगी ने बताया कि भगवान् पर ध्यान करते समय उसने भगवान् कृष्ण की बाँसुरी की ध्वनि तथा
शंख की ध्वनि सुनी। क्या यह सत्य है? यदि ऐसा है, तो इसे कैसे सुन सकते हैं?
उत्तर : यह बिलकुल सत्य है। भगवान् कृष्ण के चित्र पर धारणा करें। आप उपर्युक्त दोनों प्रकार की ध्वनि
सुनेंगे। कानों को दोनों अँगूठों से बन्द कर लें अथवा पीली मक्खी का मोम, जिसको रुई के साथ पीटा गया हो, उससे कानों को बन्द करें और दाहिने कान से आती हुई ध्वनि पर धारणा करें। आप उपर्युक्त ध्वनियों को सुनेंगे। इसका अभ्यास रात के समय करें।
प्रश्न: मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मुझे कुछ और निर्देश दें। कुछ और ध्यान की विधियाँ बतायें तथा सही
पथ पर चलने हेतु कुछ निर्देश दें।
उत्तर : भगवान् श्री कृष्ण के आभूषणों, रेशमी पीताम्बर, बाँसुरी आदि को नेत्र बन्द करके देखने का प्रयास
करें। प्रतिबिम्ब को स्थिर रखें। यदि मन भागे तथा यदि आप इसे लक्ष्य पर वापस न ला सकें, तो इसे थोड़ी देर तक घूमने दें। यह कुछ देर तक इधर-उधर कूदने के बाद स्वयं ही स्थिर हो जायेगा।
प्रश्न : हमें ध्यान हेतु समय क्यों देना चाहिए? भगवान् हमारी प्रार्थना की कामना नहीं करता, तो ऐसा करने
की आवश्यकता क्या है?
उत्तर : जीवन का लक्ष्य है आत्म-साक्षात्कार या भगवद्-साक्षात्कार। हमारे सभी कष्ट, जन्म, वृद्धावस्था तथा
मृत्यु मात्र भगवद्-साक्षात्कार के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। साक्षात्कार मात्र भगवान् पर ध्यान द्वारा ही किया जा सकता है। मेरे प्रिय राम! इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसलिए व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। भगवान् हमें प्रार्थना, जप आदि हेतु तत्पर करता है; क्योंकि भगवान् वह प्रेरक है, जो हमारे मनों को प्रेरित करता है।
प्रश्न: क्या मैं ध्यान के समय भगवान् से सहायता प्राप्त कर सकता हूँ?
उत्तर : हाँ, अन्तर्वासी की उपस्थिति जो आपके हृदय में प्रकाशित हो रही है, वह सच्चे भक्त को आलिंगन
करने हेतु अपने हाथ को फैलाये प्रतीक्षारत है।
प्रश्न: क्या रात्रि के समय भोजन के बाद ध्यान किया जा सकता है? एक गृहस्थ शाम के समय बहुत अधिक
व्यस्त रहता है, इस कारण उसे इस समय ध्यान हेतु कठिनाई से ही समय मिल पाता है।
उत्तर : रात के समय ध्यान की एक दूसरी बैठक अत्यन्त आवश्यक है। यदि मिनटों के लिए अर्थात् १० या १५
मिनट तक ध्यान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको रात्रि के समय पर्याप्त समय है, आप रात्रि को बिस्तर पर जाने के पूर्व कुछ आध्यात्मिक संस्कारों में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक संस्कार आपके लिए बहुमूल्य या अनमोल खजाना है। और आपको रात में बुरे स्वप्न भी नहीं आयेंगे। सोते समय दैवी विचार साथ रहेंगे। वहाँ अच्छे संस्कार होंगे।
प्रश्न: जप और ध्यान में क्या अन्तर है?
उत्तर : जप भगवान् का नाम बिना बोले दोहराना है। ध्यान में ईश्वर के एक ही विचार का निरन्तर प्रवाह है।
जब आप दोहरायेंगे - 'ॐ नमो नारायणाय', तो यह विष्णु-मन्त्र का जप है। जब आप विष्णु भगवान् के हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म, उनके कुण्डलों, सिर पर मुकुट, उनके रेशमी पीताम्बर आदि के बारे में विचार करेंगे, तो यह ध्यान है। जब आप भगवान् के गुण जैसे सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि के बारे में विचार करेंगे, तो यह भी ध्यान है।
प्रश्न: ध्यान कैसे करना चाहिए? इस बारे में व्यावहारिक निर्देश दीजिए।
उत्तर : एक एकान्त कमरे में पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जायें। सिर, गर्दन तथा धड़ एक सीध में हों।
अपने नेत्र बन्द कर और कल्पना करें कि एक बड़ा देदीप्यमान सूर्य आपकी हृदय गुहा में प्रकाशित हो रहा है। भगवान् विष्णु के चित्र को एक कमल के पुष्प के केन्द्र में स्थापित करें। इस चित्र को अब देदीप्यमान सूर्य के केन्द्र में देखें। 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्र का मानसिक रूप से जप करें तथा अपने हृदय में उनके सम्पूर्ण चित्र को सिर से पैर तक तथा उनको हाथों में अस्त्र लिये मानसिक रूप से देखिए। सभी अन्य सांसारिक विचारों को बन्द कर दें।
प्रश्न : जब मैं ध्यान करता हूँ, तो सिर भारी हो जाता है। इसे कैसे दूर करूँ?
उत्तर : सिर में आँवले का तेल लगायें और शीतल जल से स्नान करें। जब आप ध्यान हेतु बैठें, उससे पूर्व सिर
पर शीतल जल के छींटे दें। आप ठीक हो जायेंगे। मन के साथ संघर्ष न करें।
प्रश्न: क्या एकान्त आवश्यक है?
उत्तर : पूर्ण आवश्यक है। यह अनिवार्य है।
प्रश्न : मुझे कितने समय तक एकान्त में रहना चाहिए।
उत्तर : पूरे तीन वर्षों तक।
प्रश्न: क्या आप मुझे ध्यान हेतु कुछ एकान्त स्थान बता सकते हैं?
उत्तर : ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल, नासिक, उत्तरकाशी, बद्रीनारायण, वृन्दावन, मथुरा, अयोध्या या
कश्मीर ।
प्रश्न : मैं एकान्त जीवन हेतु स्वयं को कैसे तैयार करूँ?
उत्तर : अपनी सम्पत्ति को अपने तीनों पुत्रों में बाँट दीजिए। थोड़ा अपने जीवन-यापन हेतु अपने पास रखें।
इसका एक अंश दान में दे दें। ऋषिकेश में एक कुटीर बनाइए और वहाँ निवास करिए। अपने तीनों पुत्रों के साथ किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार न करें। समतल प्रदेशों में न प्रवेश करें। तत्पश्चात् ध्यान प्रारम्भ करें। अब आपका मन शान्ति में विश्राम करेगा। इस कार्य को तत्काल करें। आपको शीघ्रता करनी चाहिए।
प्रश्न : जब मैं उत्तरकाशी में था, तो मेरी अच्छी निष्ठा, श्रेष्ठ वृत्तियाँ एवं उत्तम धारणा थी। अब मैं साधना
भी करता हूँ; किन्तु जब से मैंने समतल प्रदेश में प्रवेश किया है, तब से मैंने उन्हें खो दिया है। ऐसा क्यों? मेरा पूर्व की भाँति उत्थान कैसे हो सकता है ?
उत्तर : सांसारिक बुद्धि वाले मनुष्य के साथ सम्पर्क तत्काल मन को प्रभावित करता है। विक्षेप भीतर आ जाते
हैं। मन अनुकरण करता है। बुरी सुविधाभोगी आदतों का विकास हो जाता है। बुरा वातावरण तथा बुरी संगत साधकों के मन पर बुरा प्रभाव उत्पन्न करने में आश्चर्यजनक भूमिका अदा करते हैं। पुराने संस्कार पुनर्जीवित हो उठते हैं। मैं आपसे तुरन्त भाग कर उत्तरकाशी चले जाने के लिए कहूँगा। एक क्षण की भी देरी न कीजिए। चूँकि मन भोजन के सूक्ष्म अंश से निर्मित है, इस कारण यह उस मनुष्य से जुड़ जाता है, जिससे यह अपना भोजन प्राप्त करता है। किसी के बन्धन में न आयें। स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करें। आत्म-निर्भर रहें।
अध्याय ५
ध्यान के प्रकार
१. ध्यान हेतु चुनाव
ध्यान के विभिन्न अनेक प्रकार है। एक विशेष प्रकार एक विशेष मन हेतु अनुकूल होता है। ध्यान का प्रकार रुचि, स्वभाव, क्षमता एवं व्यक्ति के मन के प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। एक भक्त अपने इष्टदेवता पर ध्यान करता है। एक राजयोगी विशेष पुरुष या ईश्वर (जिसे कष्टों, कामनाओं तथा कर्मों का स्पर्श भी नहीं होता) पर ध्यान करता है। एक हठयोगी चक्रो तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं पर ध्यान करता है। ज्ञानी स्वयं की आत्मा पर ध्यान करता है। जो आपको अनुकूल आये, ऐसे ध्यान का प्रकार आपको स्वयं ही खोजना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सके, तो आप आत्म-साक्षात्कार प्राप्त गुरु से सम्पर्क करें। वे आपके मन की प्रकृति तथा आपके लिए ध्यान की सही विधि जान सकते हैं।
मन जिस विषय को देखता है, उसका रूप ग्रहण कर लेता है और इसी कारण उस विषय को देखना सम्भव होता है। भक्त निरन्तर अपने इष्टदेवता का ध्यान करता है। ऐसा करने से मन सदैव इष्टदेवता का रूप ले लेता है और जब वह अपने ध्यान में स्थापित हो जाता है, तो वह सर्वत्र मात्र अपने इष्टदेवता को देखता है। नाम और रूप नष्ट हो जाते है। भगवान् कृष्ण का भक्त सर्वत्र मात्र कृष्ण को ही देखता है और गीता में वर्णित स्थिति ‘वासुदेवः सर्वमिति’—‘प्रत्येक वस्तु मात्र वासुदेव ही है' का अनुभव करता है। एक ज्ञानी अथवा एक वेदान्ती सर्वत्र मात्र अपनी आत्मा के दर्शन करता है। नाम तथा रूप का यह जगत् उसकी दृष्टि से नष्ट हो जाता है। वह उपनिषदों के ऋषियों के वचन 'सर्व खल्विदं ब्रह्म'–'सभी वास्तव में ब्रह्म हैं' का अनुभव करता है।
ध्यान के दो मुख्य प्रकार हैं—सगुण ध्यान तथा निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान में योगाभ्यासी भगवान् कृष्ण, राम, शिव, हरि, गायत्री अथवा श्री देवी के रूप पर धारण करता है। निर्गुण ध्यान में वह अपने मन की सम्पूर्ण ऊर्जा भगवान् अथवा आत्मा के एक विचार पर केन्द्रित करता है तथा स्मृति एवं अन्य सभी विचारों की तुलना करने से बचता है। एक ही विचार सम्पूर्ण मन को आपूरित कर लेता है।
जब खुले नेत्रों से भगवान् कृष्ण के स्थूल चित्र को देखते हैं और उसका ध्यान है, तो यह सगुण ध्यान है। जब आप नेत्र बन्द करके भगवान् कृष्ण का चित्र देखते है, तो यह भी सगुण ध्यान है; लेकिन यह अधिक निर्गुण है। जब आप अनन्त, निर्गुण प्रकाश का ध्यान करेंगे, तो यह और अधिक निर्गुण ध्यान है। पूर्व वाले दोनों प्रकार ध्यान के संगुण प्रकार से सम्बद्ध है और बाद वाला निर्गुण ध्यान का प्रकार है। निर्गुण में भी मन को केन्द्रित करने के लिए प्रारम्भ में एक स्थूल रूप होता है। बाद में यह रूप नष्ट हो जाता है तथा ध्याता और ध्येय एक बन जाते हैं।
सगुण ध्यान मूर्ति या भगवान् के रूप पर ध्यान है। भक्त स्वभाव वाले लोगों के लिए यह ध्यान का सगुण प्रकार है। यह भगवान् के गुणों पर ध्यान है। भगवान् के नाम ॐ का जप करें। उनके गुणों सर्वविद् सर्वज्ञ, सर्वव्यापकता आदि के बारे में विचार करें की आपका मन पवित्रता से पूर्ण हो जायेगा। भगवान् को अपने हृदय कमल पर दैदीप्यमान प्रकाश के मध्य स्थापित करें। बार-बार इस विधि को दोहरायें
कल्पना करें कि एक सुन्दर बगीचा है, जिसमें सुन्दर-सुन्दर फूल लगे हुए हैं। उसके एक कोने में सुन्दर गुलाब है। दूसरे कोने में रातरानी है। तीसरे कोने में चम्पा के फूल है। चौथे कोने में चमेली के फूल है। सर्वप्रथम चमेली पर ध्यान करें, उसके बाद मन गुलाब पर लेकर जायें, उसके बाद रातरानी पर, तत्पश्चात् मन की चम्पा के फूलों पर लेकर जायें । पुनः मन की उपयुक्त अनुसार घुमायें। इसे बार-बार १५ मिनट तक दोहराये। इस प्रकार स्थूल ध्यान करने पर यह मन को सूक्ष्म निर्गुण ध्यान हेतु तैयार करेगा।
अपने सामने ॐ का चित्र रखें। इस पर धारणा करें। खुली आँखों से त्राटक भी करें। यह दोनों ही प्रकार का ध्यान है—सगुण और निर्गुण । ॐ के चित्र को अपने ध्यान के कमरे में रखें। आप इस ब्रह्म के प्रतीक की पूजा कर सकते हैं। इसके सामने धूप-बत्ती कर सकते हैं। फूल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करना आधुनिक पढ़े-लिखे लोगों को अनुकूल होता है।
निर्गुण ब्रह्म पर निर्गुण ध्यान है। ॐ मन्त्र का जप भाव सहित मानसिक रूप से करें । सत्-चित्-आनन्द, पवित्रता, पूर्णता, मैं सर्व आनन्द हूँ आदि के विचार संयुक्त करें ।
वहाँ कोई संसार नहीं है। न वहाँ मन है न शरीर वहाँ मात्र एक ही चैतन्य (शुद्ध चेतना) है। मैं वह शुद्ध चेतना हूँ। यह निर्गुण ध्यान है। महावाक्यों पर ध्यान ॐ पर ध्यान के समतुल्य है। आप या तो 'अहं ब्रह्मास्मि' 'मैं ब्रह्म हूँ अथवा 'तत्त्वमसि' 'तू वह है' को भी ले सकते हैं। ये सभी उपनिषदों के महावाक्य है। उनके महत्त्व पर ध्यान करें। कोशों को तोड़ दें अथवा नकार दे एवं उस एक सार के साथ मिल जाये जो कि उसके पीछे निहित है।
ध्यान करें। मन को शुद्ध करें। एक एकान्त कमरे में ध्यान करें। उसके बाद उपनिषदों तथा गीता के सार को अपने हृदय से निचोड़े। अपूर्ण व्याख्याओं पर निर्भर न रहें। यदि आप लगनशील हैं, तो आप उपनिषदों के ऋषियों तथा भगवान् कृष्ण के सच्चे विचारों को समझ सकेंगे तथा यह भी कि जब शास्त्रों में इन श्लोकों को लिखा गया था, तो उनका वास्तव में क्या अर्थ था?
धारणा एवं ध्यान के द्वारा अपने हृदय में छिपी दिव्यता को अनावृत करे अपना समय व्यर्थ न गँवायें। अपना जीवन व्यर्थ न गँवायें। ध्यान करें, ध्यान करें। एक क्षण भी व्यर्थ न गँवायें। ध्यान जीवन के समस्त कष्टों का उन्मूलन करेगा। यही एकमात्र रास्ता है। ध्यान मन का शत्रु है। यह मनोनाश लाता है।
ध्यान दो प्रकार का होता है—सगुण तथा निर्गुण। यदि आप एक स्थूल विषय के किसी चित्र पर ध्यान करते हैं, तो यह सगुण है। यदि आप किसी निर्गुण विचार या किसी गुण (जैसे करुणा, सहनशीलता आदि) पर ध्यान करते हैं, तो यह निर्गुण ध्यान है। नवाभ्यासी को सगुण ध्यान करना चाहिए। कुछ के लिए निर्गुण ध्यान सगुण ध्यान से अधिक सरल होता है।
साधक को प्रत्याहार (इन्द्रियों पर संयम) तथा धारणा में निपुण होने के बाद ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यदि इन्द्रियाँ उपद्रवी है, यदि मन एक बिन्दु पर एकाग्र नहीं है, तो १०० वर्षो में भी किसी प्रकार ध्यान सम्भव नहीं है। व्यक्ति को अवस्था से अवस्था तक चरण दर चरण आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएँ कम करनी चाहिए तथा मन की सभी प्रकार की बेकार, जंगली कामनाओं को त्याग देना। चाहिए। एक निष्काम पुरुष ही मात्र शान्त बैठ सकता है और ध्यान कर सकता है। सात्विक, हल्का आहार तथा ब्रह्मचर्य ध्यान के अभ्यास हेतु पूर्वपक्षाएँ है।
चेतना दो प्रकार की है—केन्द्रित चेतना तथा सतही चेतना। जब आप त्रिकुटी पर धारणा करते हैं, तो आपकी केन्द्रित चेतना त्रिकुटी पर होती है। जैसे जब कोई मक्खी ध्यान के समय आपके बायें हाथ पर बैठ जाती है, तो आप उसे दाहिने हाथ से भगाते हैं, जब आप मक्खियों के प्रति चैतन्य होते हैं, तो यह सतही चेतना कहलाती है।
एक बीज जो अग्नि में एक सेकेंड के लिए भी रह जाता है, वह निस्सन्देह अंकुरित नहीं हो सकता चाहे वह उर्वरा भूमि में ही क्यों न बोया गया हो। उसी प्रकार एक मन जोकुछ समय के लिए ध्यान करता है, लेकिन अस्थिरता के कारण विषय-वस्तुओं की ओर भागता है, वह योग के पूर्ण परिणाम नहीं प्राप्त कर सकता ।
२. विभिन्न पथों में ध्यान
ध्यान दो प्रकार का है— सगुण तथा निर्गुण। धारणा के बाद ध्यान आता है।
निदिध्यासन के दीर्घकालीन अभ्यास के पश्चात् समाधि सहज और स्वाभाविक बन जाती है, किन्तु ऐसा प्राणायाम अथवा किसी हठयोग के अभ्यास से सम्भव नहीं हो रुकता।
एक राजयोगी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार एवं धारणा के अभ्यास सहजता से ध्यान भाव में प्रवेश कर जाता है। भक्त ऐसा भगवान् के प्रति शुद्ध प्रेम के भाव से करता है। एक वेदान्ती अथवा ज्ञानयोगी चतुस्साधनों के अर्जन, श्रुतियों के श्रवण तथा श्रवण किये हुए पर मनन के द्वारा ध्यान के भाव में प्रविष्ट हो जाता है। एक हटयोगी गहन एवं निरन्तर प्राणायाम के अभ्यास से ध्यान-भाव में प्रविष्ट होता है।
भगवान् हरि के चतुर्भुज रूप अथवा भगवान् कृष्ण के मुरलीधर रूप अथवा भगवान राम के धनुष-बाण हाथ में लिये हुए रूप पर ध्यान करें। यह स्थूल ध्यान सगुण ध्यान है। शान्ति पर ध्यान करें। यह निर्गुण या सूक्ष्म ध्यान है। ध्यान करें— “मैं शान्ति का मूर्तिमान स्वरूप हूँ।” यह वेदान्तिक निर्गुण ध्यान या अहंग्रह उपासना है। आनन्द पर ध्यान करें। यह भी निर्गुण ध्यान है। अपने स्वभाव, रुचि, क्षमता या प्रवृत्ति, व्यवस्था के अनुसार किसी भी ध्यान के प्रकार का चुनाव कर लें तथा इसी जन्म में जीवन के लक्ष्य पर पहुँचें।
ध्यान दो प्रकार का होता है—जप सहित ध्यान अर्थात् जप को संयुक्त करके ध्यान तथा जप रहित ध्यान अर्थात् जप के बिना ध्यान अथवा मात्र शुद्ध ध्यान । जब आप 'ॐ नमो नारायणाय' मानसिक या वैखरी रूप से दोहरायेंगे, तो यह मात्र जप है। जब आप शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बर, कंगन आदि सहित भगवान् हरि के रूप ध्यान करते हुए इस मन्त्र का जप करेंगे, तो यह जप सहित ध्यान है। जब आप ध्यान मैं प्रगति करेंगे, तो जप स्वयं ही छूट जायेगा। आप मात्र ध्यान करेंगे। यह जप रहित ध्यान कहलाता है।
जिस प्रकार एक दीप में ज्योति जलती है, उसी प्रकार अनादि काल से दैवी ज्योति आपके हृदय-दीप में जल रही है। अपने नेत्र बन्द करें। स्वयं को दिव्य ज्योति में लीन करें। अपने हृदय की गहन गुहा में डूब जाये। दिव्य ज्योति पर ध्यान करें तथा भगवान् की ज्योति बन जायें।
इन्द्रियों को विषयों से वापस खींच लें। अपने परम तप से भगवान् को प्रसन्न करें । भगवान् हरि पर ध्यान करें, दैदीप्यमान दिव्य विमान में बैठ जायें और भगवान् विष्णु के परम धाम पहुँचें।
हे मित्रो! जागें, अब और न सोयें। ध्यान करें। अब यह ब्राह्ममुहूर्त है। अपने हृदय में स्थित भगवान् के मन्दिर के द्वार को प्रेम की चाबी से खोलें। आत्मा का संगीत सुनें । अपने प्रिय को प्रेम का गीत सुनायें। अनन्त का मधुर संगीत बजायें। अपने मन को उनके ध्यान में विलीन कर दें। उनके साथ एक हो जायें। स्वयं को आनन्द एवं प्रेम के सागर में डुबा दें।
ये वे चिह्न हैं जो यह बतायेंगे कि आप ध्यान तथा भगवान् के पास पहुँचने में विकास कर रहे हैं। आपको संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा। विषय-वस्तुएँ आपको अब और नहीं ललचायेंगी। आप निष्काम, निर्भय, 'मैं' रहित, 'मेरा' रहित बन जायेंगे। देहाध्यास अर्थात् शरीर के प्रति मोह धीरे-धीरे कम होता जायेगा। 'वह मेरी पत्नी है', 'वह मेरा पुत्र है', 'यह मेरा घर है' – आप इन विचारों पर ध्यान नहीं देंगे। आप अनुभव करेंगे कि सभी भगवान् के प्रकट स्वरूप हैं। आप प्रत्येक वस्तु में ईश्वर के दर्शन करेंगे।
मन तथा शरीर हल्के हो जायेंगे। आप सदा प्रसन्न और उत्साहपूर्ण रहेंगे। भगवान् का नाम सदा आपके होठों पर रहेगा। मन सदा भगवान् के चरणों पर केन्द्रित रहेगा। मन सदा भगवान् का चित्र बनाता रहेगा। यह सदा भगवान् के चित्र देखेगा। आप वास्तव में ऐसा अनुभव करेंगे कि सत्त्व अथवा पवित्रता, प्रकाश, आनन्द तथा ज्ञान सदैव ईश्वर से आपकी ओर प्रवाहित हो रहे हैं और आपके हृदय को आपूरित कर रहे हैं।
मानव की अभिलाषा का अन्तिम लक्ष्य राजयोग दर्शन के संस्थापक पतंजलि महर्षि के अनुसार भगवान् के साथ मिलन नहीं, बल्कि आत्मा का पदार्थ से पूर्ण कैवल्य है।
मन को शान्त बनायें। बुद्धि को स्थिर बनायें। इन्द्रियों को स्थिर करें। अब आप गहन ध्यान में प्रवेश करेंगे। जागरूक बने। रजोगुण भीतर प्रवेश करने का प्रयास करेगा। इस घुसपैठिये को निर्दयतापूर्वक मारें तथा पुनः शान्तता प्राप्त करें।
योग में दृष्टि को भीतर निर्दिष्ट किया जाता है। बाहर की ओर जाती हुई इन्द्रियों एवं मन को निरन्तर साधना द्वारा योगी संयमित करता है। योगी वृत्तियों या मन की लहरों को नियन्त्रित करता है और परिणाम स्वरूप असम्प्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि में विश्राम करता है। उसे वृत्तियों के नियन्त्रण में बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समुद्र की लहरें इन कठिनाइयों के सामने कुछ भी नहीं है। अत्यन्त जागरूक निर्भीक योगी इस शरीर रूपी जहाज (जो कि भयंकर भव-सागर में हिचकोले खा रहा है) का कप्तान है। वह निरन्तर धारणा तथा ध्यान द्वारा मन की लहरों को रोक देता है और अभयता तथा अमरता के दूसरे किनारे पर पहुँच जाता है।
जब आप आध्यात्मिक लक्ष्य या निर्विचार अवस्था पर पहुँच जायेंगे, तो आप अमरता, अनन्त शान्ति एवं परमानन्द के धाम पर पहुँच जायेंगे। राम अब अपने घर की और वापसी की यात्रा प्रारम्भ करो। आध्यात्मिक पथ पर साहस के साथ चलो। कठिनाइयों से न डरो। साहसी बनो। एक-एक करके शिखर के बाद शिखर पर चढ़ते जाओ। मार्ग में आने वाले सूक्ष्म मोह तथा अहंकार की गहन कन्दरा को पार कर लो। लम्बी कूद लगाओ और युद्ध की रहस्यमय दीवार को फाँद जाओ। अब शुद्ध आनन्द एवं सर्वोच्च ज्ञान के अनन्त राज्य में प्रवेश करो। अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करो, दैवी वैभव को पुनः प्राप्त करो। अपने सत्-चित्-आनन्द स्वरूप में विश्राम करो।
विचारों की प्रकृति तथा शक्ति को समझो और स्वीकार करो। उत्कृष्ट श्रेष्ठ विचारों का भी अतिक्रमण कर लो और निर्विचार अवस्था में प्रवेश करो। स्वयं को शुद्ध चेतना के साथ एक कर दो। यहाँ तक कि एक अत्यन्त पापी मनुष्य भी यदि एक क्षण के लिए भी अमर आत्मा पर ध्यान करता है, तो वह महान् पवित्र सन्त बन जाता है।
प्रारम्भ में मन को स्थूल विषय या प्रतीक पर केन्द्रित करके मन को संयमित किया जाता है। जब यह स्थिर और सूक्ष्म हो जाता है, तो यह बाद में एक निर्गुण विचार जैसे 'अहं ब्रह्मास्मि' पर केन्द्रित किया जा सकता है।
सदा ध्यान करें - "मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं सत्-चित्-आनन्द ब्रह्म हूँ। मैं निर्विकार स्वप्रकाश्य अमर आत्मा हूँ। मैं तीनों अवस्थाओं— जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं का साक्षी हूँ। मैं शरीर, मन, प्राण एवं इन्द्रियों से पृथक् हूँ। मैं पंच कोश से पृथक् हूँ।" आप आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। आपको आत्मज्ञान (ब्रह्मज्ञान) प्राप्त होगा।
एक यति को सदैव उस भाव पर ध्यान करना चाहिए, जिसे निद्रा के एकदम पहले अथवा जाग्रत अवस्था की समाप्ति पर अनुभव किया जाता है। वह मात्र इसके द्वारा ही मुक्त हो सकता है। यही निस्संकल्प या निर्द्वन्द्व अवस्था प्राप्ति हेतु एकमात्र अवलम्बन है।
एक कामना मन में उत्पन्न होती है। यह सन्तुष्ट हो जाती है। तत्पश्चात् अन्य कामना उत्पन्न हो जाती है। दोनों कामनाओं के मध्य के अन्तराल में मन की पूर्ण स्थिरता होती है। मन की दो वृत्तियों के मध्य के इस अन्तराल अथवा सन्धि में पूर्ण शान्ति रहती है।
जब मन ब्रह्म (परमात्मा) पर एकाग्र होता है, तो यह ब्रह्म के साथ एक बन जाता है जैसे अग्नि के साथ कपूर या पानी के साथ नमक या दूध के साथ जल एक बन जाता है। तब वहाँ कोई द्वैत नहीं होता। ध्यानकर्ता ब्रह्म बन जाता है। यह कैवल्य स्थिति है।
यह ब्रह्माण्ड, मनुष्य तथा तीनों देव-ब्रह्मा, विष्णु और शिव ॐ में निहित हैं। सभी वेद तथा षड्दर्शन ॐ में निहित हैं। ॐ ही सब कुछ है। ॐ ब्रह्म है । ॐ पर अर्थ और भाव सहित ध्यान करें। ब्रह्म को जानें और मुक्त हो जायें।
आपको ध्यान की ६ अवस्थाओं को पार करना होगा तथा अन्त में आप पूर्ण निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करेंगे। रूप-दर्शन पूर्णतया नष्ट हो जायेगा। अब वहाँ न तो ध्यान होगा न ध्येय। ध्याता और ध्येय एक हो गये हैं। आप सर्वोच्च ज्ञान तथा अनन्त परम शान्ति प्राप्त करेंगे। यह जीवन का परम लक्ष्य है। अब आप ज्ञान प्राप्त जीवन्मुक्त हैं। आप जीवित रहते हुए मुक्त हैं। इसलिए अब आप जीवन्मुक्त हैं। आप दर्द, दुःख, भय, सन्देह तथा मोह से पूर्ण मुक्त हैं। आप ब्रह्म से एक हो गये हैं। बुलबुला समुद्र बन गया है। नदी समुद्र में मिल गयी है और समुद्र बन गयी है। सभी भेद तथा उपाधियाँ पूर्णतया नष्ट हो गयी हैं। आप अब अनुभव करेंगे- में ब्रह्म हूँ, सर्वत्र और कुछ नहीं मात्र ब्रह्म है।" - "मैं अमर आत्मा हूँ, सभी वास्तव में ब्रह्म हैं, सर्वत्र और कुछ नहीं मात्र ब्रह्म है ।''
अखण्ड ब्रह्म-भाव को बनाये रखने का प्रयास करें। ॐ में उड़े। इस स्थिति को जितनी अधिक देर तक बनाये रख सकें, रखें। उसमें स्थापित हो जायें। सदैव सहज अवस्था (स्वाभाविक ब्रह्म-भाव) बनाये रखें। अब यही आपका लक्ष्य और प्रयत्न होना चाहिए।
३. प्रारम्भिक ध्यान
(अ) गुलाब के फूल पर ध्यान
किसी स्थूल या निर्गुण विचार पर मन को स्थिर करने को धारणा कहते हैं। ध्यान धारणा से सिद्ध होता है। जिस पर धारणा की जा रही है, उस पर अखण्ड, अटूट सतत विचार-प्रवाह ध्यान है। अप्रशिक्षित चित्त के लिए प्रारम्भ में किसी विषय का स्थूल ध्यान आवश्यक होता है। एक कमरा ऐसा हो जो ध्यान के लिए ही नियत हो। उसमें पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन पर बैठिए और गुलाब के फूल का ध्यान कीजिए. अर्थात् गुलाब के फूल का रंग-रूप, उसके विभिन्न अंग दल, डण्ठल, पराग आदि का ध्यान कीजिए। श्वेत, पीला, लाल आदि विविध रंगों के गुलाबों का ध्यान कीजिए। गुलाब-जल, गुलाब-अर्क, इत्र, गन्ध, गुलकन्द आदि गुलाब से निर्मित विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान कीजिए। यह ध्यान कीजिए कि गुलाब-जल का उपयोग नेत्र-प्रदाह में होता है। गुलकन्द का उपयोग कब्ज-निवारण में होता है। गुलाब के फूल और फूल-माला का उपयोग भगवान् की अर्चना में तथा केशों को सजाने के लिए किया जाता है। फिर उसके विभिन्न गुणों का ध्यान कीजिए जैसे शरीर में उससे शीतलता मिलती है, उसमें वायु विकार का नाश करने की शक्ति है। गुलाब एवं गुलाब की मालाओं के मूल्य के बारे में विचार कीजिए। अब उन स्थानों का ध्यान कीजिए जहाँ गुलाब अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। इस प्रकार गुलाब से सम्बन्ध रखने वाली और भी अनेक बातों पर ध्यान कीजिए। ध्यान रखिए, गुलाब के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ से सम्बन्धित विचार ध्यान में न आयें। इस प्रकार के स्थूल विषय पर ध्यान के अभ्यास से चित्त सूक्ष्म ध्यान करने के योग्य हो जाता है। एक महीने तक प्रातः पाँच बजे इसका अभ्यास आधे घण्टे तक कीजिए।
(आ) भैंस पर ध्यान
नर्मदा-तीर पर स्थित ओंकारेश्वर के कृष्णचैतन्य नामक एक ब्रह्मचारी ने श्रीरामाचार्य के पास जा कर प्रार्थना की कि वे उसे ध्यान प्रक्रिया सिखायें। श्रीरामाचार्य ने कहा- "हे कृष्ण! तुम श्री कृष्ण भगवान् की उस मूर्ति का ध्यान करो जो मुरलीधर है, पैर तिरछे रख कर खड़े हैं, विशाल सूर्य-मण्डल के मध्य तुम्हारे हृदय-कमल में स्थित है और इसके साथ ही प्रसिद्ध कृष्ण-मन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का मानसिक जप करो।” कृष्णचैतन्य ने कहा- -"गुरु जी ! मैं बिलकुल मन्द-बुद्धि हूँ। मुझसे यह नहीं होगा। यह मेरे लिए बड़ा कठिन है। मन्त्र भी बहुत लम्बा है। कृपया मुझे और कोई सरल पद्धति बतलाइए। '
रामाचार्य ने कहा कृष्णचैतन्य! डरो नहीं। मैं तुम्हे सरल पद्धति बताता हूँ। सुनो। अपने सामने श्रीकृष्ण की पीतल की छोटी-सी मूर्ति रख लो। पद्मासन में बैठो। स्थिर दृष्टि से उस मूर्ति के हाथ, पैर आदि विभिन्न अंगों को ध्यान से देखो। किसी अौर 'वस्तु की ओर न देखो।" कृष्णचैतन्य ने कहा- "गुरु जी ! यह तो और भी कठिन है। पालथी लगा कर बैठना बड़ा कठिन है। इससे पिण्डली दुखती है। जब पीड़ा की ओर ध्यान जाता है, तब मूर्ति की ओर दृष्टि नहीं जाती। मुझे स्थिर बैठना है, ध्यान से मूर्ति को देखना है और उसके प्रत्येक अंग का अवलोकन करना है। मैं एक समय में एक से अधिक काम नहीं कर सकता और दो वस्तुओं से अधिक स्मरण नहीं रख सकता है गुरु महाराज! मुझे कोई बहुत ही सुगम मार्ग बताइए। "
रामाचार्य ने कहा—“चैतन्य! अपने सामने पिता का चित्र रख लो। उसके सामने चाहे जिस आसन में बैठो। थोड़ी देर तक उस आकृति को केवल देखते रहो।" कृष्णचैतन्य ने उत्तर दिया—‘“गुरु जी! मेरे स्वामी! यह भी कठिन है, क्योंकि मुझे अपने पिता जी से बड़ा डर लगता है। वे बड़े भयंकर हैं। वे मुझे खूब पीटते हैं। उनके उस रूप के स्मरण से ही मैं काँप उठता हूँ, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। यह मेरे लिए कदापि उपयुक्त न होगा। मैं तो यह कहूँगा कि यह तो पहले वालों से भी अधिक कठिन है। अतः गुरु जी! मेरी प्रार्थना है कि कृपा कर इस बार बहुत ही सरल विधि बतलाइए। मैं अवश्य ही उसका अभ्यास करूँगा।"
रामाचार्य ने पूछा – “कृष्ण! मुझे अब बताओ कि तुम्हें सबसे प्रिय क्या वस्तु लगती है?” कृष्ण ने उत्तर दिया – “गुरु जी ! मैंने घर में एक भैंस पाल रखी है। उससे मुझे खूब दूध, दही तथा घी मिलता है। मुझे वह सबसे अधिक प्रिय है। उसका स्मरण मुझे सदा आता रहता है।” तब रामाचार्य ने कहा-"कृष्ण! तुम इस कमरे में जाओ और दरवाजा बन्द कर लो। एक कोने में चटाई पर बैठ कर अपने मन को दूसरी चीजों से - हटा कर उस भैंस का ही सतत ध्यान करो और अन्य कोई बात न सोचो। इसी समय इसका अभ्यास करो। "
अब कृष्णचैतन्य बड़ा प्रसन्न हुआ। वह प्रसन्न मन से कमरे में गया और उसने गुरु के आदेशों का अक्षरशः पालन किया तथा गम्भीरता से एकाग्रतापूर्वक अपनी भैंस का ध्यान करने लगा। वह लगातार तीन दिनों तक अपने आसन से नहीं उठा।
वह खाना-पाना भूल गया। उसे अपने शरीर का और परिस्थितियों का भान नहीं रहा वह केवल भैंस के विचार में गम्भीरता से तल्लीन रहा। तीसरे दिन रामाचार्य कृष्णचैतन्य की स्थिति देखने के लिए उसके कमरे में गये और देखा कि वह ध्यान में मग्न है जोर से आवाज दे कर गुरु जी ने पूछा- क्यों कृष्ण! कैसा लग रहा है? बाहर आओ, खाना खा लो। कृष्णचैतन्य ने उत्तर दिया- "गुरु जी! आपके प्रति मैं बड़ा " कृतज्ञ हूँ। इस समय मैं गम्भीर ध्यान में हूँ। अब मैं बाहर नहीं आ सकूँगा। में बहुत बड़ा हूँ। मेरे सिर पर सींग निकल आये हैं। मैं इस छोटे-से दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता। मैं भैंस को बहुत चाहता हूँ। मैं स्वयं भैंस बन गया हूँ।"
रामाचार्य ने देखा कि कृष्ण का मन एकाग्रता को प्राप्त कर चुका है और अब वह समाधि के योग्य हो गया है। उन्होंने कहा— कृष्ण! तुम भैंस नहीं हो। अब अपना ध्यान बदल दो। भैंस के नाम और रूप को भूल जाओ और उस नाम रूप के पीछे निहित सारतत्त्व, जो सच्चिदानन्द है, जो तुम्हारा ही निज-स्वरूप है, उसका ध्यान करो ।" कृष्णचैतन्य ने अपने ध्यान की प्रक्रिया बदल दी और गुरु जी के उपदेश पर चल कर जीवन के ध्येय रूप कैवल्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया।
उपर्युक्त कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी वस्तु पर ध्यान करना सुगम होता हैं जो हमारे मन को सबसे अधिक प्रिय हो ।
पतंजलि महर्षि ने ध्यान के अनेक प्रकार बताये हैं जैसे "विशोका वा ज्योतिष्मती” – हृदय-कमल में स्थित ज्योतिस्वरूप वस्तु जो कि शोक रहित है, उसका ध्यान करो (१-३६)। “वीतरागविषयं वा चित्तम्"- '—उस चित्त का ध्यान करो और जो ऐन्द्रिक विषयों से अनासक्त है" (१-३७)। “स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा" - स्वप्न तथा निद्रावस्था में अनुभव किये जाने वाले ज्ञान का ध्यान करो (१-३८) और उन्होंने अन्त में " यथाभिमतध्यानाद्वा" अथवा जो तुम्हें प्रिय हो, उसका ध्यान करो (१-३९) सूत्र प्रस्तुत किया है। जो विषय मन को अत्यन्त प्रिय हो, उस पर ध्यान करना सरल होता है।
(इ) महात्मा गान्धी पर ध्यान
अपने ध्यान-कक्ष में जाइए। पद्मासन में बैठिए। गान्धी जी के रंग, रूप, आकार, ऊँचाई आदि का ध्यान कीजिए। इंग्लैंड में उनकी पढ़ायी, अफ्रीका में उनकी वकालत, अफ्रीकी भारतीयों की स्थिति सुधारने की उनकी राजनैतिक गतिविधियाँ, भारत में उनका उत्कट असहयोग आन्दोलन, उनका प्रसिद्ध चरखा और खादी, देश-भर में खादी को लोकप्रिय बनाने का उनका व्यापक विचार, हिन्दू-मुसलिम एकता हेतु उनके अथक प्रयत्न, पतित अस्पृश्यों के उत्थान के कार्य, उनके उच्च आदर्श तथा सिद्धान्त, उनका त्यागमय जीवन, संन्यास-वृत्ति, उनका त्याग और कठोर तपश्चर्या का जीवन, उनके आहार सम्बन्धी संयम, मानसिक ब्रह्मचर्य की निरन्तर साधना, वाणी, कर्म विचारों में अहिंसा और सत्य का आदर्श, उनकी पत्रकारिता की सहज लेखन क्षमता, अँगरेजी, हिन्दी तथा गुजराती में उनकी कई उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन, उनके द्वारा उस उपयोगी आश्रम की स्थापना जहाँ उत्तम कर्मयोगियों का प्रशिक्षण चलता है, उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति तथा उनके अन्य सद्गुणों का ध्यान कीजिए। कोई दूसरा विचार मन में नहीं आने देना चाहिए। मन भागता हो, तो उसे खींच लाइए और उसे उपर्युक्त विचारों में स्थिर कीजिए। दो मास तक प्रतिदिन आधे घण्टे तक इसका अभ्यास कीजिए आपको ध्यान की ठीक विधि ज्ञात हो जायेगी।
(ई) बारह गुणों पर ध्यान
इन बारह गुणों पर दस-दस मिनट तक ध्यान कीजिए :
१. जनवरी में नम्रता
२. फरवरी में आर्जव
३. मार्च में साहस
४. अप्रैल में धैर्य
५. मई में करुणा
६. जून में उदारता
७. जुलाई में सच्चाई
८. अगस्त में शुद्ध प्रेम
९. सितम्बर में दानशीलता
१०. अक्तूबर में क्षमा
११. नवम्बर में समता
१२. दिसम्बर में सन्तोष
शुद्धता, उत्साह, साहस तथा प्रसन्नता का भी विकास कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपमें वास्तव में ये सभी गुण विद्यमान हैं। स्वयं से कहिए मैं धैर्यवान् हूँ। आज से मैं चिड़चिड़ा नहीं बनूँगा। मैं अपने दैनिक जीवन में इस सद्गुण को व्यक्त करूंगा। मैं उन्नति कर रहा हूँ। इस सद्गुण धैर्य के लाभों पर विचार कीजिए। अधैर्य से होने वाली हानियों का भी चिन्तन कीजिए। इसी प्रकार आप सभी सद्गुणों का विकास कर सकते हैं।
(उ) भजनों पर ध्यान
यदि आप गायन कला में निपुण है, तो एकान्त स्थान में जाइए। जी भर कर मधुरता से गाइए तथा अपने हृदय स्थल से राग-रागिनियों को दिल खोल कर निकालिए। स्वयं अपने को, अपने अतीत को तथा परिस्थितियों को भूल जाइए। यह ..एक सरल उपाय है। कुछ स्तोत्र, भजन और दार्शनिक गीत चुन लीजिए। तुकाराम के अभंग, गुजराती में आखा भजन के गीत, तमिल में तायुमान स्वामी के भजन और तेवारम् के तमिल के भजन तथा हिन्दी में ब्रह्मानन्द भजनमाला इसके लिए विशेष उपयुक्त हैं। बंगाल के एक प्रसिद्ध सन्त रामप्रसाद ने इस विधि से साक्षात्कार किया था। रावण ने अपने शरीर के स्नायुओं के तन्तुओं के द्वारा सामगान के द्वारा भगवान् शिवजी को प्रसन्न किया था। संगीत के विषय में शेक्सपियर के विचार सुनिए— “जो मनुष्य संगीत नहीं जानता या सुमधुर संगीत से आनन्दित नहीं होता, वह द्रोह, छल और सर्वनाश कर सकता है। उसकी भावनाएँ अन्धकार के समान कालिमायुक्त होती हैं और उसका प्रेम अधोलोक के समान तमिस्र होता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।” देखिए, गायन विद्या का महत्त्व! आप गायन के द्वारा मन को सरलता से विषयों से वापस खींच सकते हैं। गायन तत्काल मन का उत्थान करता है और मन का विस्तार करता है। एक विस्तृत मन को सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म पर एकाग्र करना सरल होता है। जो चाहिए है, वह है उत्तम रुचि तथा संगीत में योग्यता और हृदय की पवित्रता तथा ध्यान का स्थिर अभ्यास ।
(ऊ) गीता श्लोकों पर ध्यान
भगवद्गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों को कण्ठस्थ कर लीजिए। आसन पर बैठ कर मन में उनका पारायण कीजिए ।
१. गीता के द्वितीय अध्याय में 'आत्मा की अमरता से सम्बन्धित कुछ प्रमुख श्लोक हैं। इन विचार
श्रृंखलाओं पर आप धारणा और ध्यान कर सकते हैं। आपको यह अभ्यास अत्यन्त उपयोगी प्रतीत होगा।
२. द्वितीय अध्याय में वर्णित स्थितप्रज्ञावस्था के लक्षणों का ध्यान कीजिए।।
३. षष्ठम अध्याय के ध्यानयोग के प्रभाव की विचार श्रृंखला पर ध्यान कीजिए।
४. त्रयोदश अध्याय में वर्णित श्लोक, जो ज्ञानी के गुण की व्याख्या करते हैं, उन विचार - शृंखलाओं का
ध्यान कीजिए।
५. उन श्लोकों से प्राप्त विचार-श्रृंखलाओं का ध्यान कीजिए जिनमें दैवी सम्पत्ति की प्रकृति का वर्णन है।
६. एकादश अध्याय में वर्णित विश्वरूप-दर्शन के विचार पर ध्यान कीजिए।
७. द्वादश अध्याय में 'यो मद्भक्तः स मे प्रियः' श्लोक पर ध्यान कीजिए।।
८. चतुर्दश अध्याय में वर्णित 'गुणातीत पुरुष के लक्षणों का ध्यान कीजिए।
मैंने आपके सम्मुख विचारों के आठ समूह प्रस्तुत किये हैं। इनमें से किसी एक को, जो आपको प्रिय लगे, चुन लीजिए। आप मन को एक विचार के बाद दूसरे विचार पर भी ले जा सकते हैं।
४. सगुण ध्यान
(अ) इष्टदेवता पर ध्यान
यह भगवान् कृष्ण, राम, सीता या देवी की मूर्ति पर ध्यान है। यह भक्ति-मार्ग के लोगों के लिए ध्यान का स्थूल रूप है। यह भगवान् के गुणों के साथ ध्यान है। उनके नाम का जप भी करें। उनके गुण — सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता आदि के बारे में विचार करें, आपका मन पवित्रता से भर जायेगा। भगवान् कृष्ण का मुरली हाथ में लिये तथा भगवान् विष्णु का शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथ में लिये चित्र स्थूल ध्यान हेतु उत्तम हैं। उनको चमकदार प्रकाश के मध्य अपने हृदय पर सिंहासनारूढ़ करें। उनके चरणकमलों, पीताम्बर, कौस्तुभ मणि सहित हार, कर्ण-कुण्डल, मुकुट, बाजूबन्द, शंख, चक्र, गदा और पद्म के बारे में मानसिक रूप से विचार करें। उसके बाद पुनः उनके चरणकमलों पर आ जायें। इस विधि को बार-बार दोहरायें।
रूप-विशेष पर ध्यान सगुण ध्यान कहलाता है। अपनी रुचि या स्वभाव के अनुरूप शिव, विष्णु, राम अथवा कृष्ण की मूर्ति, जो भी आपको अत्यन्त प्रिय हो, चुन लीजिए अथवा अपने गुरु के निर्देशों का पालन करें। गुरु आपके लिए कोई इष्टदेव चुन देंगे। वह इष्ट आपको मार्ग दिखायेगा। शर-सन्धान करने वाला पहले स्थूल तथा बड़े लक्ष्य को ले कर बाण चलाता है। उसके बाद कोई मध्यम लक्ष्य अपनाता है। अन्त में वह सूक्ष्म लक्ष्य को बेधता है। ठीक उसी प्रकार साधक को प्रारम्भ में सगुण ध्यान करना चाहिए और चित्त के भली-भाँति प्रशिक्षित तथा अनुशासित हो जाने पर वह निर्गुण, निराकार पर ध्यान कर सकता है। स्थूल विषय का ध्यान सगुण ध्यान है। सूक्ष्म विषय का ध्यान निर्गुण ध्यान है। सगुण उपासना से विक्षेप दूर होता है। तीन या छह महीने तक किसी चित्र पर त्राटक कीजिए।
छह महीने तक त्राटक का अभ्यास करने के बाद त्रिकुटी पर (भ्रूमध्य भाग पर) मूर्ति के मानसिक चित्र का आधे घण्टे से दो घण्टे तक ध्यान कीजिए। फिर यह अनुभव कीजिए कि विश्व की समस्त वस्तुओं में आपके इष्ट उपस्थित हैं। अपने इष्टदेव के मन्त्र का जप कीजिए। इष्टदेवता के सर्वशक्तिमानता, सर्वज्ञता आदि गुणों का चिन्तन कीजिए। अनुभव कीजिए कि सात्त्विक गुण इष्टदेव से आपकी ओर प्रवाहित हो रहे हैं और वे सात्त्विक गुण आपमें विद्यमान हैं। यह सात्त्विक या शुद्ध भावना है। इस प्रकार से साधना कीजिए। इससे एकाग्रता की साधना में सहायता मिलती है। मूर्ति के विभिन्न अंगों को मानसिक रूप से देखते जाइए। मान लीजिए, चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति सामने है, उस पर निम्न प्रकार से ध्यान कीजिए। त्राटक कीजिए । त्राटक का अभ्यास सगुण ध्यान में बहुत ही उपयोगी है।
ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः ।
केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी
हारी हिरण्मयवपुः धृतशंखचक्रः ॥
शंखचक्रगदापने द्वारकानिलयच्युत ।
“भगवान् नारायण का, द्वारका के अविनाशी अच्युत का सदा ध्यान करें जो सूर्य मण्डल के मध्य स्थित हैं, कमलासन पर विराजमान हैं, केयूर, मकर-कुण्डल, किरीट और हार धारण किये हुए हैं, जिनका शरीर स्वर्णमय है तथा जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारी हैं।"
ध्यानावस्था में विष्णु भगवान् के अंग-प्रत्यंगों का विचार कीजिए। मन ही मन पहले उनके चरणों को देखिए, फिर जानु प्रदेश पर ध्यान कीजिए। इसी क्रम से उनका पीताम्बर, हृदय प्रदेश पर कौस्तुभ मणि जड़ित हार, कानों में मकर कुण्डल, मुखकमल, मस्तक पर मुकुट, दाहिने ऊपरी हाथ में चक्र, बायें ऊपरी हाथ में शंख, दाहिने निचले हाथ में गदा और बायें निचले हाथ में कमल-पुष्प का ध्यान कीजिए। यह ध्यान का क्रम है। फिर नीचे चरणों में जाइए और ऊपर तक इसी तरह ध्यान करते हुए चलिए। इस प्रक्रिया से चित्त बाह्य विषयों से विमुख हो जाता है।,
पहले विराट् पुरुष का ध्यान करें, फिर सगुण रूप ले और अन्त में निर्गुण का ध्यान करें।
(आ) विराट् पुरुष पर ध्यान
अपने ध्यान कक्ष में पद्मासन अथवा सिद्धासन पर बैठिए और प्रतिदिन आधे घण्टे तक निम्नांकित विचारों का ध्यान कीजिए। यह प्राथमिक साधकों के लिए छह महीने तक करने योग्य स्थूल ध्यान-प्रक्रिया है।
१. स्वर्ग उनका शीर्ष है।
२. पृथ्वी उनके पाद हैं।
३. दिशाएँ उनके हाथ हैं।
४. सूर्य-चन्द्र उनके नेत्र हैं।
५. अग्नि उनका मुख है।
६. धर्म उनका पृष्ठ है।
७. वनस्पति उनके केश हैं।
८. पर्वत उनकी अस्थियाँ हैं।
९. सागर उनका मूत्राशय है।
१०. नदियाँ उनकी नाड़ियाँ हैं।
ऐसा करने पर चित्त विकसित होगा। तब भगवान् राम, कृष्ण या शिव के रूप में सगुण ध्यान आरम्भ कीजिए। इस प्रकार एक वर्ष तक ध्यान कीजिए। उसके पश्चात् । ब्रह्म के निर्गुण ध्यान का आश्रय लीजिए। इन विभिन्न प्रणालियों से अभ्यास करने पर बिन सूक्ष्म ध्यान के योग्य बनेगा और उसमें सूक्ष्म विचार करने की क्षमता आयेगी।
(इ) गायत्री पर ध्यान
गायत्री वेदों की माता है। यह चराचर प्राणियों के स्वामी ईश्वर की प्रतीक है। गायत्री मन्त्र के जप से चित्त शुद्धि होती है, जिसके बिना आप अध्यात्म मार्ग में कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी तनिक भी आध्यात्मिक उन्नति सम्भव नहीं है। गायत्री एक प्रभावशाली विश्व-प्रार्थना है। यह ब्रह्म गायत्री के नाम से भी प्रसिद्ध है।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ परब्रह्म
भूः भूलोक
भुवः अन्तरिक्ष
स्वः स्वर्गलोक
तत् ब्रह्म, परमात्मा
सवितुः ईश्वर, विधाता
वरेण्यं पूजनीय
भर्गः अज्ञाननाशक
देवस्य देव का
धीमहि हम ध्यान करते हैं।
धियो बुद्धि
यो जो
न: हमारी
प्रचोदयात् प्रेरणा दे
"उस ईश्वर और उसकी महिमा का हम ध्यान करते हैं, जिसने विश्व की सृष्टि की है, जो पूजनीय है, जो समस्त पाप और अज्ञान का नाश करने वाला है, वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे!"
सूर्योदय के समय स्नान करके ध्यान कक्ष में जायें। अपने आसन पर बैठ कर इस मन्त्र का कम से कम १०८ बार जप करें और निरन्तर यह भावना करे कि देवी गायत्री से आपको ज्योति, शुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो रहा है। गायत्री मन्त्र के अर्थ का मनन करें। यह नितान्त आवश्यक है। त्रिकुटी पर, भ्रूमध्य पर दृष्टि केन्द्रित करें।
५. निर्गुण ध्यान
(अ) विचारों पर ध्यान
यह निर्गुण ब्रह्म का ध्यान है। यह अहंग्रह उपासना है। यह ॐ का ध्यान है। यह निराकार विषय का ध्यान है। पद्मासन पर बैठिए। ओंकार का मानसिक जप कीजिए । मन में निरन्तर उसके अर्थ का चिन्तन कीजिए यह अनुभव कीजिए कि आप सर्व अनन्त प्रकाश है। अनुभव कीजिए कि आप शुद्ध सच्चिदानन्द व्यापक आत्मा है, नित्य शुद्ध सिद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हैं। अनुभव कीजिए कि आप चैतन्य हैं। अनुभव कीजिए कि आप अखण्ड, परिपूर्ण, एकरस, शान्त, अनन्त, नित्य, अपरिवर्तनीय सत्ता है। यह विचार आपके कण-कण में, अणु-परमाणु में, नस-नस में और रग-रग में व्याप्त होना चाहिए, स्पन्दित होना चाहिए। ॐ का उच्चारण मात्र अधिक लाभकर नहीं होगा। यह आपके हृदय से, बुद्धि से तथा आत्मा से निकलना चाहिए। आपको सर्वात्म भाव में यह अनुभव होना चाहिए कि आप सूक्ष्म, सर्वव्यापी, चैतन्य रूप हैं और यह भावना हर समय बनी रहनी चाहिए।
ॐ का मानसिक जप करते समय देह भावना का निषेध करें। ॐ का उच्चारण करते समय यह भावना रखें :
मैं अनन्त हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं सर्वज्योति हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं सुखस्वरूप हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं तेजोमय हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं शक्तिस्वरूप हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं ज्ञानस्वरूप हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं आनन्दस्वरूप हूँ ॐ ॐ ॐ
उपयुक्त विचारों का सतत चिन्तन कीजिए उत्साह तथा लगन के साथ निरन्तर प्रयास इसमें परम आवश्यक तत्व है। उपर्युक्त विचारों को मन ही मन अविरत गति से दोहराते जायें, तो साक्षात्कार होगा। आपको २ या ३ वर्षों में आत्म-दर्शन हो जायेगा।
निर्गुण ध्यान अथवा वेदान्तिक साधना में अत्यन्त महत्त्व रखने वाले दो तत्त्व हैं- एक इच्छा और दूसरा मनन। मनन से पूर्व श्रवण आता है। श्रवण का अर्थ है श्रुतियों को मनन के बाद निदिध्यासन आता है। निदिध्यासन का अर्थ उत्साह और लगन का निरन्तर बने रहना है। गम्भीर ध्यान का नाम ही निदिध्यासन है। निदिध्यासन से साक्षात्कार अथवा अपरोक्षानुभूति होती है। जिस प्रकार खूब तपे हुए लोहे पर गिरने वाली बूँद लोहे में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चित्त तथा आभास चैतन्य ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। चिन्मात्र, चैतन्य मात्र शेष रह जाता है। वेदान्त-साधना के श्रवण, और निदिध्यासन पतंजलि महर्षि के राजयोग के धारणा, ध्यान और समाधि के समान हैं।
उपासना, ध्यान तथा मन्त्र-जप में चित्त उपास्य या ध्येय का ही रूप धारणा कर लेता है और उतने समय के लिए ध्येय अर्थात् इष्टदेवता की शुद्धि इसमें भी आ जाती है। अभ्यास से मन इसकी शुद्धता में स्थिर हो जाता है और फिर मलिनता की ओर नहीं जाता है। जब तक मन का अस्तित्व है, तब तक उसे एक न एक विषय चाहिए ही और वह साधना का विषय ऐसा हो जो शुद्ध हो।
मन्त्र जप की जो ध्वनि है, वह इस प्रकार सुमधुर तथा निरन्तर होनी चाहिए जो जप-विषय का अर्थात् देवता का साक्षात्कार करा सके। पुनः पुनः उच्चारण करने से संस्कार की शक्ति के द्वारा मन्त्र में सृजक गतिशीलता का होता है।
समाधि में चित अपनी चेतना खो देता है और ध्येय के साथ एकाकार (तदाकार तद्रूप) हो जाता है। ध्याता और ध्येय, उपासक और उपास्य, चिन्तक और चिन्त्य एक हो जाते हैं। विषयी और विषय, अहम् (मैं) और इदम् (यह ), द्रष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। प्रकाश और विमर्श मिल कर एक हो जाते हैं। एकता, तद्रूपता, तदाकारता, एकात्मता, समता ही निर्विकल्प समाधि है ।
विचारों के संचरण के रूप में, सत्ता रूप में, अपने ही अस्तित्व के रूप में, ब्रह्म रूप में निर्विकल्प समाधि के दो प्रकार हैं। एक वह जिसमें ज्ञानी समस्त विश्व को अपने अन्दर ही देखता है। वह स्वरूप विश्रान्ति अर्थात् ब्रह्म में विश्राम करना कहलाता है। ब्रह्म विश्व को अपने अन्दर अपने ही संकल्प या विवर्त के रूप में देखता है। ज्ञानी भी यही करता है। यह साक्षात्कार की परमोच्च अवस्था है। इस अवस्था में भगवान् श्री कृष्ण, भगवान् दत्तात्रेय, श्री शंकराचार्य, ज्ञानदेव आदि पहुँचे थे।
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥
"जो योगयुक्त पुरुष है, वह अपने को समस्त भूर्ती में तथा समस्त भूतों को अपने में देखता है और वह सर्वत्र समदर्शी होता है" (गीता ६-२९) । किन्तु जिसे साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है, वह विश्व को अपने से भिन्न, स्वतन्त्र तथा बाह्य वस्तु के रूप में देखता है। इसका कारण अविद्या है।
निर्विकल्प समाधि के दूसरे प्रकार में रज्जुसर्प न्याय के अनुसार ज्ञानी की दृष्टि से विश्व लुप्त हो जाता है, वह शुद्ध निर्गुण ब्रह्म में अवस्थित होता है। राजयोगी सविकल्प समाधि से छूटने के बाद ब्रह्माकार-वृत्ति के द्वारा निर्गुण ब्रह्म में ज्ञानी की अवस्था को प्राप्त कर लेता है।
एक जीवित विश्व-शक्ति अथवा ज्ञान है जो सभी नाम-रूपों के पीछे सन्निहित है। यह शक्ति अथवा ज्ञान, जो निराकार है, के ऊपर ध्यान करें। यह प्रारम्भिक निराकार निर्गुण ध्यान का निर्माण करेगा। यह परम निर्गुण निराकार चेतना के साक्षात्कार की ओर प्रेरित करेगा।
पद्मासन में बैठ जायें। वायु पर धारणा करें। यह नाम और रूप रहित ब्रह्म एक जीवित सत्य का साक्षात्कार हेतु प्रेरित करेगा।
कल्पना करें कि एक परम अखण्ड अनन्त ज्योति है, जो कि इस सम्पूर्ण गोचर पदार्थों के पीछे छिपी है, जिसकी ज्योति करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के बराबर है। इस पर ध्यान करें। यह एक अन्य प्रकार का निर्गुण ध्यान है।
विस्तृत फैले आकाश पर ध्यान करें। यह एक अन्य प्रकार का निर्गुण निराकार ध्यान है। धारणा में पूर्व की विधियों के द्वारा मन सीमित रूपों के बारे में विचार करना बन्द कर देगा। धीरे-धीरे यह शान्ति के समुद्र में विलीन हो जायेगा। यह अपने निहित विषयों जैसे विभिन्न प्रकार के रूपों से रहित हो जायेगा। यह सूक्ष्मातिसूक्ष्म भी बन जायेगा।
निर्गुण ब्रह्म पर असम्बद्ध ध्यान को निर्गुण ध्यान कहते हैं। ॐ का भाव सहित मानसिक जप करें। सत्-चित्-आनन्द, शुद्धता, पूर्णता, 'मैं सर्व आनन्द हूँ, मैं स्वरूप हूँ, मैं असंगोऽहं हूँ, मैं अनासक्त हूँ, केवलोऽहं, मैं अकेला हूँ, अखण्ड एक रस- चिन्मात्रोsहं' के विचारों को संयुक्त कीजिए।
(आ) वेदान्तिक ध्यान
यह मात्र निर्गुण ध्यान है। निम्न वाक्यों पर ध्यान करें
मैं सब हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं सब में सब हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं सबके भीतर अमर आत्मा हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं जीवित सत्य हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं जीवित यथार्थता हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं तीनों कालों का साक्षी हूँ ॐ ॐ ॐ
(अहं साक्षी अवस्थात्रय - साक्षी)
मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ ॐ ॐ ॐ
(निराकार ज्योति-स्वरूपोऽहं)
मैं सूर्यों का सूर्य हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं परम सत्ता, परम ज्ञान, परमानन्द हूँ ॐ ॐ ॐ
(सत्-चित्-आनन्द-स्वरूपोऽहं)
अवतारवादियों के निराकार वेदान्तिक ध्यान में भी साधना के प्रारम्भ में भी एक स्थूल प्रतीक होता है।
भविष्य में यह प्रतीक नष्ट हो जायेगा। जब आप ध्यान करें, तो तीनों शरीरों को नकार दें और स्वयं को अन्तर्निहित सार के साथ एक करें। नाम एवं रूपों को अस्वीकार करें। भौतिक शरीर अथवा मन, प्राण, बुद्धि अथवा इन्द्रियों को शुद्ध अनन्त आत्मा की भाँति समझने की गलती न करें। सर्वोच्च आत्मा उपर्युक्त मायावी साधनों अथवा मायावी पदार्थों से बिलकुल पृथक् है। इस बात का भली प्रकार स्मरण रखें। उपर्युक्त वाक्यों पर ध्यान करें तथा काम के समय भी यही भावना बनाये रखें। आप अपनी रुचि के अनुसार कोई एक वाक्य ले सकते हैं। यदि मन घूमे, तो मन को बार-बार बिन्दु पर वापस ले कर आये। यदि मन भटके, तो आप मन को एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर घुमायें और अन्त में जब यह स्थिर हो जाये, तो इसे एक वाक्य पर एकाग्र करे। अब मन इस प्रकार स्थिर हो जायेगा जैसे एक निर्वात स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है। यह एक वाक्य भी स्वयं ही गुम हो जायेगा। आप अपने स्व स्वरूप शुद्ध आनन्द की निर्विचार अवस्था में विश्राम करेंगे। समाधि अथवा परम चेतनावस्था अब प्रकट होगी। आत्मा के आनन्द का अनुभव करें। आन्तरिक आनन्द का अनुभव करें।
(इ) वेदान्तिक निदिध्यासन के लिए संकल्प
मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं पूर्ण शुद्ध हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं पूर्ण आनन्द हूँ ॐ ॐ ॐ
मैं सर्वव्यापक चेतना हूँ ॐ ॐ ॐ
सच्चिदानन्द स्वरूपोऽहं ॐ ॐ ॐ
अखण्ड एकरस चिन्मात्रोऽहं ॐ ॐ ॐ
भूमानन्द स्वरूपोऽहं ॐ ॐ ॐ
अहं साक्षी (मैं साक्षी हूँ) ॐ ॐ ॐ
निर्विशेष- चिन्मात्रोऽहं ॐ ॐ ॐ
असंगोऽहं (मैं अनासक्त हूँ) ॐ ॐ ॐ
जीवन्मुक्त की महिमा अवर्णनीय है। वह स्वयं ही ब्रह्म है। आठों सिद्धियाँ और नौ ऋद्धियाँ उसके चरणों में लोटती हैं। सत् संकल्प के द्वारा वह चमत्कार कर सकता है धन्य हैं वे जीवन्मुक्त जो कि इस पृथ्वी पर धन्य आत्मा हैं। उनका आशीर्वाद आप सब पर हो!
(ई) वेदान्तिक धारणा
मन को सभी विषय वस्तुओं से खींचने के द्वारा हृदय के भीतर गहरे गोते लगाये। इस क्षुद्र ‘मैं' को मार दें और जानें कि 'मैं वह हूँ' (सोऽहं)। जिस प्रकार जल की बूँद अपना नाम और रूप खो देती है और समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जीव स्वयं को परमात्मा में विलीन कर देता है और अपना नाम तथा रूप खो देता है।
यदि आप एक बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं और यदि आप सदैव यात्रा करते रहते हैं, तो आपको ध्यान हेतु किसी विशेष कमरे तथा विशेष समय की आवश्यकता नहीं है। श्वास के साथ 'सोऽह का जप और ध्यान कीजिए अथवा आप श्वास के साथ राम-मन्त्र संयुक्त कर सकते हैं। तब प्रत्येक श्वास प्रार्थना अथवा ध्यान बन जायेगी। सोऽहं अथवा राम का स्मरण रखिए। उनकी सर्वत्र उपस्थिति का अनुभव कीजिए। इतना ही पर्याप्त होगा।
यदि मन निरन्तर विषय-वस्तुओं में लीन रहता है, तो जगत् की सत्यता की धारणा में अवश्य ही वृद्धि होगी। यदि मन निरन्तर आत्मा के बारे में विचार करता रहता है, तो यह ससार एक स्वप्न की भाँति प्रतीत होता है। स्वयं को मन के आधारभूत विचारों, विभिन्न निरर्थक संकल्पों (परिकल्पनाओं) से मुक्त रखें।
निरन्तर आत्मा की खोज करें। निरन्तर विचारों पर ध्यान दें। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। ऐसा करने पर ही मात्र आध्यात्मिक ज्ञान का प्रारम्भ होगा।
वेदान्त अथवा ज्ञान के पथ में 'मनन' तथा 'निदिध्यासन' शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता | विजातीय-वृत्ति-तिरस्कार (सांसारिक विषयों के सभी विचारों को दूर भगाना) तथा स्वजातीय-वृत्ति-प्रवाह (भगवान् अथवा ब्रह्म की विचार-तरंगों में एक स्थिर धारा की भाँति वृद्धि करना) मनन कहलाता है। निदिध्यासन गहन प्रबल ध्यान है। यह अन्तर्मुख-वृत्ति-निरोध अथवा आत्माकार-वृत्ति-स्थिति है। इस समय मन परमात्मा में पूर्ण स्थित रहता है। इस समय कोई भी सांसारिक विचार अनधिकृत प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय ध्यान तेल की स्थिर धारा (तैलधारावत् (प्रवाह) की भाँति होता है।
प्रारम्भ में जब आप नवाभ्यासी होते हैं तो चूँकि आप अत्यन्त दुर्बल होते हैं, इसलिए आप मन के विचलन को रोकने के लिए नेत्र बन्द कर सकते हैं। लेकिन बाद में आपको नेत्र खुले रख कर यहाँ तक कि पैदल चलते समय भी ध्यान करना चाहिए। आपको सारे समय मन का सन्तुलन बनाये रखना चाहिए, अन्यथा पूर्णता-प्राप्ति की कोई आशा नहीं है। इस दृश्यमान जगत् के अनस्तित्व पर सदैव ध्यान करते रहें। आत्मा का मात्र अस्तित्व है।
सभी दृश्यमान वस्तुएँ माया है। माया आत्मा पर ध्यान अथवा ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जायेगी। व्यक्ति को स्वयं को माया से मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। माया का विनाश मन के द्वारा हो सकता है। मन के विखण्डन का अर्थ है माया को दूर हटाना। ध्यान माया पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है।
वास्तव में मन के कर्म ही हैं जिन्हें कर्म कहा जाता है। मन की दासता से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। जिन्होंने स्वयं को अपने मन की चंचलता से मुक्त कर लिया है, उन्हें परम निष्ठा (ध्यान) की प्राप्ति होती है। मन को इसकी समस्त अशुद्धिया से शुद्ध होना चाहिए तब यह अत्यन्त शान्त बनेगा, तब इसके जन्म और मृत्यु के सारे सांसारिक भ्रामक सहायक शीघ्र नष्ट हो जायेंगे। यदि आप एक कुत्ते के सामने एक बड़ा दर्पण रखें और उसके सामने एक रोटी का टुकड़ा रख दें, तो कुत्ता सबसे पहले दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देख कर उसे भौंकेगा। वह मूर्खतापूर्वक कल्पना करेगा कि दूसरी ओर एक अन्य कुत्ता बैठा हुआ है। इसी प्रकार मनुष्य अपने मन रूपी दर्पण के द्वारा सभी लोगों में अपना प्रतिबिम्ब मात्र देखता है और कुत्ते की भाँति मूर्खतापूर्वक कल्पना करता है कि वे उससे अलग हैं और ईर्ष्या तथा द्वेष के कारण झगड़ा करता है।
“कोई जगत् नहीं है, न शरीर है न मन। वहाँ मात्र एक चैतन्य (शुद्ध चेतना) है। मैं वह शुद्ध चेतना हूँ।” यह निर्गुण ध्यान है।
निदिध्यासन (ध्यान) में आपको स्वजातीय-वृत्ति प्रवाह का विकास करना होगा। ब्रह्म अथवा दैवी चेतना के विचारों के प्रवाह को सतत बनाये रखिए। विजातीय-वृत्ति का तिरस्कार कीजिए। विषयों के विचारों को त्याग दीजिए। विवेक और वैराग्य के कोड़े से उन्हें दूर भगा दें। प्रारम्भ में संघर्ष होगा। यह वास्तव में थका देने वाला होगा। लेकिन बाद में जैसे-जैसे आप दृढ़ और अधिक दृढ़तर होते जायेंगे और जैसे-जैसे आप शुद्धता में तथा ब्रह्मचैतन्य में विकास करेंगे, वैसे-वैसे आपकी साधना सरल होती जायेगी, तब आप एकता के जीवन में आनन्द लेंगे। आप आत्मा से शक्ति प्राप्त करेंगे। जब विषय-वृत्तियाँ तनु हो जाती हैं तथा मन एकाग्र हो जाता है, तो आन्तरिक शक्ति में वृद्धि होती है।
स्वयं को अनन्त, शुद्ध, अमर आत्मा, जो आपके हृदय के भीतर निवास करती है, के साथ एक करने का प्रयत्न कीजिए। सदैव विचार करें और अनुभव करें कि मैं सर्व शुद्ध आत्मा हूँ। यही एक विचार आपकी सभी कठिनाइयों एवं काल्पनिक विचारों को दूर कर देगा। मन आपको भ्रमित करना चाहता है। विचारों के प्रवाह के इस अवरोधक को प्रारम्भ कीजिए। मन एक चोर की भाँति छुप जायेगा।
(उ) ॐ पर ध्यान
जो इस नश्वर जीवन के असीम सागर में गिरे हुए हैं, उनके लिए ॐ एक नाव के समान है। इस नाव की सहायता से अनेकों ने इस संसार सागर को पार किया है। यदि आप भाव तथा अर्थ सहित ॐ पर ध्यान करें, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और आत्म-साक्षात्कार कर सकते हैं।
ॐ अमर सर्वव्यापक आत्मा अथवा आत्मा का एकमात्र प्रतीक है। हर चीज़ को बाहर निकाल कर एकमात्र ॐ का ही विचार करें। सभी नाशवान् विचारों को बन्द कर दे। वे बार-बार प्रकट होंगे । शुद्ध आत्मा के विचारों को बार-बार उत्पन्न कीजिए। शुद्धता, पूर्णता, मुक्ति, ज्ञान, अमरता अनन्तता, नित्यता आदि के विचारों को संयुक्त कीजिए। ॐ का मानसिक जप कीजिए।
ॐ ही प्रत्येक वस्तु है। ॐ ही ईश्वर का, ब्रह्म का प्रतीक है। ॐ आपका वास्तविक नाम है। ॐ मनुष्य के तीनों प्रकार के सभी अनुभवों को आच्छादित करता है। ॐ इस सम्पूर्ण दृश्यमान जगत् का प्रतीक है। ॐ से ही यह विषय जगत् निकला है। यह विश्व ॐ में ही अस्तित्वमान है और ॐ में ही विलीन हो जाता है। 'अ' इस भौतिक धरातल को अभिव्यक्त करता है, 'उ' मानसिक तथा सूक्ष्म जगत्, आत्माओं के जगत् तथा स्वर्ग लोकों को, 'म' गहन निद्रावस्था तथा वह सब जो आपकी जाग्रत अवस्था में भी अज्ञात है, वह सब जो बुद्धि से परे है, को अभिव्यक्त करता है। ॐ सबको अभिव्यक्त करता है। ॐ आपके जीवन, विचारों तथा बुद्धि का आधार है।
सभी शब्द जो विषयों को निर्दिष्ट करते हैं, वे सभी ॐ में केन्द्रित हैं। इस कारण यह संसार ॐ से आया है, ॐ में स्थित रहता है और ॐ में विलीन हो जाता है।
ॐ ब्रह्म अथवा परमात्मा का प्रतीक है। ॐ पर ध्यान करें। जब आप ॐ पर ध्यान करें अथवा ॐ के बारे में विचार करें, तो आपको उस ब्रह्म के बारे में (जो कि इस प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त होता है) विचार करना है।
ॐ के साथ संयोग इसके अर्थ के साथ एक बन जाता है। "तज्जपस्तदर्थभावनम्।” जब आप ॐ के बारे में विचार करें अथवा ॐ का ध्यान को अथवा ॐ का उच्चारण करें, तो स्वयं को सर्व आनन्दमयी आत्मा के साथ एक करने का प्रयत्न करें तथा पंचकोश को माया के द्वारा निर्मित भ्रामक संयोग की भाँति कारें। आपको ॐ के प्रतीक को सत् चिद् आनन्द ब्रह्म अथवा आत्मा की भाँति लेना चाहिए। यह अर्थ है। ध्यान के समय आपको अनुभव करना चाहिए कि आप सर्व शुद्धता, सर्व प्रकाश, सर्वव्यापक अस्तित्व आदि है। आत्मा पर नित्य ध्यान करें। विचार करें कि आप मन और शरीर से भिन्न है। अनुभव करें: "मैं सत्-चित्-आनन्द आत्मा हूँ मैं सर्वव्यापक आत्मा हूँ। " यह वेदान्तिक ध्यान है।
ॐ पर तब तक ध्यान करें, जब तक आप समाधि न प्राप्त कर लें। यदि आपका मन रजस् तथा तमस् से विचलित हो, तो धारणा और ध्यान का बार-बार अभ्यास करते रहें।
"व्यक्ति के शरीर को अथवा निम्न आत्मा को अरणी के नीचे का भाग बना कर तथा प्रणव को अरणी का ऊपरी भाग बना कर ध्यान के अभ्यास द्वारा व्यक्ति को अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन करना चाहिए।” (श्वेताश्वतर उपनिषद्)
हे राम! अब आप हिमालय में निवास कर रहे हैं। प्रकृति भगवान् के साथ हिल-मिल कर रहें। ऊँचे शिखर आपसे अनन्त जीवन के रहस्यों को फुसफुसा कर बता रहे हैं। आपके चारों ओर बहती नदी आपको ओंकार का गीत सुनायेगी। अपने मन को प्रणव की ध्वनि पर केन्द्रित करें और उत्कृष्ट मिलन में सरलता से प्रविष्ट हो जायें। प्रकृति अपने रहस्यों को प्रकट करेगी। उससे उपदेश ग्रहण करें। बर्फ से ढँके पहाड़ों, ग्लेशियरों तथा ताजगी से पूर्ण हिमालय की वायु, सूर्य की किरणों, नीले आकाश, टिमटिमाते सितारों के साथ एकता का अनुभव करें।
आप अद्वैत ब्रह्म में विश्राम करें और अमरता के मधु का पान करें! आप जाग्रत, स्वप्न तथा गहन निद्रावस्था का अन्वेषण करके तुरीयावस्था के आनन्द की चतुर्थ अवस्था तक पहुँचें! आप सभी के पास ओंकार अथवा प्रणव की ग्राह्य बुद्धि हो! आप सभी अ उ म ध्वनियों को पार करके ध्वनि रहित ॐ में प्रविष्ट हो जायें! आप सभी ॐ का ध्यान करें तथा जीवन के लक्ष्य उस अन्तिम सत्य सत्-चित्-आनन्द ब्रह्म को प्राप्त करें! यह ॐ आपका निर्देशन करे, यह ॐ आपका निर्देश, आदर्श एवं लक्ष्य बने! माण्डूक्य उपनिषद् के रहस्य एवं सत्यों की आप पर वृष्टि हो ! ॐ ॐ ॐ !!
(ऊ) 'सोऽहं' पर ध्यान
‘सोऽहं' का अर्थ है—मैं वह हूँ, वह मैं हूँ, मैं वह ब्रह्म हूँ। 'सः' का अर्थ है-वह । 'अहं' का अर्थ है - मैं। यह सभी मन्त्रों में महान् है। यह परमहंस संन्यासियों का मन्त्र है। यह एक अभेद-बोध-वाक्य है, जो जीव की अथवा ब्रह्म अथवा परमात्मा की एकता को चरितार्थ करता है। यह मन्त्र ईशावास्योपनिषद् में आता है 'सोऽहमस्मि ।
"सोऽहं ॐ मात्र है। स और ह को हटा दें, तो आपको ॐ प्राप्त होगा। 'सोऽह' प्रणव अथवा ॐ का रूपान्तरण है। कुछ लोग ॐ से अधिक 'सोऽहं' को पसन्द करते है; क्योंकि उनको इसे श्वास के साथ संयुक्त करने में अथवा मिश्रित करने में सरलता होती है। इसके साथ ही इस मन्त्र का जप करने में किसी प्रकार का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप मात्र श्वास को देखें, तो इतना ही पर्याप्त होगा।
'सोऽह' पर ध्यान ॐ पर ध्यान के समान ही है। कुछ लोग संयुक्त मन्त्र दोहराते हैं। "हंसः सोऽहं-सोऽहं हंसः। जब आप 'सोऽहं' पर ध्यान प्रारम्भ करें, उसके पूर्व नेति नेति सिद्धान्त का अभ्यास करें। आप यह दोहरा कर "नाऽहं इदं शरीर" - "अहं एतत् न। "मैं यह शरीर, मन और प्राण नहीं हूँ। मैं वह हूँ, मैं वह हूँ-सोऽहं सोऽहं !”
इस मन्त्र का मानसिक रूप से जप करें। आप अपने सम्पूर्ण हृदय, अपनी आत्मा से यह अनुभव करें कि आप सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वानन्दमयी आत्मा अथवा ब्रह्म है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। ऐसा करने पर ही आप इस मन्त्र के जप अथवा ध्यान के परिणामों का साक्षात्कार कर सकेंगे। मात्र मानसिक रूप से दोहराना पर्याप्त नहीं होगा। इसके अपने ही लाभ हैं। लेकिन भाव में ही अधिकतम लाभ का साक्षात्कार है। भाव आत्म-साक्षात्कार है।
यदि बुद्धि यह अनुभव करने का प्रयत्न करे कि 'मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ" तथा चित्त यह अनुभव करने का प्रयत्न करे कि 'मैं मुख्य न्यायालय में क्लर्क हूँ, दुर्बल हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए धन हेतु क्या करूँगा? मुझे डर है कि न्यायाधीश मुझे दण्ड देंगे' तो साक्षात्कार सम्भव नहीं है। आपको सभी कुसंस्कारों, मिथ्या कल्पनाओं, सभी दुर्बलताओं, सभी अन्धविश्वासों तथा सभी व्यर्थ भयों को नष्ट करना होगा। यहाँ तक कि यदि आप शेर के मुख में भी फँसे हों, तब भी आपको शक्तिपूर्वक कहना है- “सोऽहं, सोऽहं, सोऽहं, मैं यह शरीर नहीं हूँ!" तभी आप सच्चे वेदान्ती होंगे। यहाँ तक कि चाहे आपके पास खाने को कुछ न हो, आप बेरोजगार हों, तो भी आपको शक्ति के साथ कहना है- “सोऽहं, सोऽहं” आप मन तथा अविद्या के कारण दूषित हो गये हैं। यह अविद्या है, यह मन है जो इस शरीर के साथ एक भाव के कारण व्यक्ति को इस सीमितता में लाया है। अज्ञानता के आवरण को चीर दें। पंचकोशों को चीर दें। अविद्या के परदे को दूर कर दें। 'सोऽहं' मन्त्र पर ध्यान के द्वारा अपने मूल सच्चिदानन्द स्वरूप में विश्राम करें।
जीव अथवा जीवात्मा २४ घण्टे में २१,६०० बार इस मन्त्र को दोहराता है। यहाँ तक कि निद्रा के समय भी यह जप स्वयं ही चलता रहता है। श्वास को बड़ी सावधानीपूर्वक देखिए। आपको ज्ञात होगा कि जब आप श्वास भीतर लेते हैं, तो 'सो' की ध्वनि उत्पन्न होती है और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो 'है' की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे अजपाजप कहते हैं, क्योंकि यह ओठों को हिलाये बिना भी ही चलता रहता है। इसका सुबह एवं सायंकाल दो घण्टे तक अभ्यास कीजिए। यदि आप इसका दस घण्टे तक नित्य जप कर सके, तो यह और भी अधिक अच्छा है। जब आप पथ में आगे बढ़ जायेंगे तो आपको चौबीस घण्टे तक ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। हंस उपनिषद् का अध्ययन करें। आपको ध्यान में सच्चा विश्राम प्राप्त होगा आपको नींद की आवश्यकता नहीं रहेगी।
"हंसः सोऽहं सोऽहं हंसः इस संयुक्त मन्त्र का अभ्यास गहरा प्रभाव डाल है। तिरुवनमलई के प्रसिद्ध स्वामी श्री शेषाद्री अक्सर इस संयुक्त मन्त्र का अभ्यास करते रहते थे। जब वे सड़क या बाजार में भ्रमण करते थे, तो इस मन्त्र को दोहराते रहते इस मन्त्र पर ध्यान करते थे। हम कहते हैं "ईश्वर प्रेम है—प्रेम ईश्वर है। इसी प्रकार ‘हंसः सोऽहं—सोऽहं हंसः’अत्यधिक बल प्रदान करता है। यह मन्त्र के बल को तीव्र करता है। साधक आत्मा से अधिक आन्तरिक शक्ति या आत्म-शक्ति प्राप्त करता है। उसका दृढ विश्वास तीव्रतर होता जाता है। इस प्रकार का जप महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्मैवाहमस्मि — मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ मैं' के जप के समान है।
सूफी फकीरों का 'अनल हक' परमहंस संन्यासियों के 'सोऽहं' के अनुरूप है। गुरु नानक इसकी बड़ी प्रशंसा करते थे।
आपका जीवन-काल योग के प्रकाश में अनेकों 'सोऽहं' के द्वारा गिना जा सकता है। यह वास्तव में अनेक वर्षों के द्वारा नहीं बना है। प्राणायाम के अभ्यास से आप 'सोऽहं' श्वास बचा सकते हैं और इस प्रकार अपने जीवन में वृद्धि कर सकते हैं। अपने अभ्यास के प्रारम्भ में बस साधारण रूप से श्वास को देखें। एक बन्द कमरे में 'सोऽहं' पर भाव एवं अर्थ सहित ध्यान करें। जब आप बैठे हों, खड़े हों, भोजन कर रहे हो, बातें कर रहे हों अथवा स्नान कर रहे हों, तब भी मौन जप करते हुए श्वास को देख सकते हैं।
‘सोऽहं' जीवन की श्वास है। ॐ श्वास की आत्मा है। 'है' को हटा दें और 'मैं' को प्रतिस्थापित करें, तो 'सोऽहं' 'मैं वह है' बन जायेगा। यदि आप श्वास पर धारणा करें, तो आप देखेंगे कि जैसे-जैसे ध्यान गहन होता जाता है, श्वास धीमी और धीमी होती जा रही है। धीरे-धीरे 'सोऽहं का जप रुक जाता है और वहाँ गहन ध्यान होता है। मन बहुत शान्त रहता है। आप आनन्दित होंगे। अन्त में आप परमात्मा के साथ एक हो जायेंगे।
(ए) महावाक्यों पर ध्यान
श्रुतियों के पवित्र वचन महावाक्य कहलाते हैं। वे चार है :
१. 'प्रज्ञानं ब्रह्म'
२. 'अहं ब्रह्मास्मि'
३. 'तत्त्वमसि'
४. 'अयमात्मा ब्रह्म'
प्रथम वाक्य ऋग्वेद के ऐतरेयोपनिषद् में है। द्वितीय वाक्य यजुर्वेद के बृहदारण्यकोपनिषद् में है। तृतीय वाक्य सामवेद के छान्दोग्योपनिषद् में और चतुर्थ अथर्ववेद के माण्डूक्योपनिषद् में है।
पहला लक्षण वाक्य है जो ब्रह्म के लक्षण का प्रतिपादन करता है और तद्बोध ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा अनुभव वाक्य है जो साक्षीज्ञान देता है। तीसरा उपदेश वाक्य है। यह शिवज्ञान प्रदान करता है।। गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं। चौथा साक्षात्कार-वाक्य है जो ब्रह्मज्ञान प्रदान करता है। आप इनमें से कोई भी महावाक्य चुन सकते हैं और उस पर ॐ के समान ही ध्यान कर सकते हैं।
'अहं ब्रह्मास्मि' पर ध्यान करें। मन में 'अहं ब्रह्मास्मि' का जप करते समय सदा ऐसी भावना कीजिए कि आप शुद्ध, सत्-चित्-आनन्द व्यापक आत्मा हैं। कोरा जप निरर्थक है। प्रत्यक्ष हृदय में वैसी भावना होनी चाहिए। इसी से आगे चल कर अनुभूति के उच्च स्तरों तक पहुँचा जा सकेगा।
कम्बल को चार तह कर बिछा दीजिए और उस पर अपने प्रिय आसन में पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठ कर सतत ध्यान कीजिए :
१. मैं अनन्त ज्योति हूँ।
२. मैं सर्वशक्तिमान हूँ।
३. मैं सर्वज्ञ हूँ।
महावाक्यों पर ध्यान ॐ पर ध्यान के सदृश है। आप 'अहं ब्रह्मास्मि अथवा 'तत्त्वमसि' महावाक्य को ले सकते हैं। उनके अर्थ पर ध्यान कर सकते हैं। अपने कोशों को नकार दें अथवा फेंक दें तथा उस सार के साथ एक हो जाये जो उनमें निहित है।
ध्यान करें और अपने मन को शुद्ध करें। इसके पश्चात् उपनिषद् अथवा गीता को अपने हृदय में से निचोड़ें। अपूर्ण व्याख्याओं पर निर्भर न रहें। यदि आप लगनशील है, तो आप उपनिषदों के ऋषियों तथा भगवान् श्री कृष्ण के सच्चे संकल्पों को समझ सकेंगे। आप जानेंगे कि जब ज्ञान से परिपूर्ण इन श्लोकों को कहा गया था, तो इनका वास्तविक अर्थ क्या था। धारणा और ध्यान के द्वारा अपने हृदय में छिपी दिव्यता को अनावृत करें। अपना समय बरबाद न करे। अपना जीवन व्यर्थ न गँवाये।
(ऐ) भावात्मक ध्यान
१. मैं सर्वत्व हूँ।
२. मैं सर्वात्मक हूँ।
उपर्युक्त विचारों पर ध्यान कीजिए। इस ध्यान में शरीर और विश्व ब्रह्मरूप और शोकमय है। यह ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति माने जाते हैं। यह सर्वथा असंगत विचार है कि ब्रह्म स्वयं आनन्दमय है और ब्रह्म का आविर्भाव रूप यह विश्व दुःख, निराशावाद त्याज्य है। समस्त दुःख और शोक के पीछे जो कुछ है, वह जीव-सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि में कहीं कोई न्यूनता या दोष नहीं है। ईश्वर की सृष्टि दुःखदायी नहीं है, बल्कि वह तो मुक्ति में सहायक है। जीव-सृष्टि में अहंकार, काम, क्रोध, मैं और मेरे का भाव, अहं कर्तृत्व भाव आदि विकार होते हैं। यही सब दुःखों का कारण है। यह अज्ञान के कारण होता है जिसमें सीमित चित्त को आप अपना निज स्वरूप समझ लेते हैं।
सर्वदा उपर्युक्त विचार को मन में दोहराते रहिए। ऐसी भावना कीजिए कि आप सर्वरूप हैं। भावना कीजिए कि समस्त शरीरों में आपकी शक्ति काम कर रही है। निरन्तर इन विचारों में लीन रहिए—‘“सारा विश्व मेरा शरीर है। सभी शरीर मेरे हैं। सभी कष्ट मेरे हैं। सभी आनन्द मेरे हैं।” ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, अहंकार आदि नष्ट हो जायेंगे। भावनात्मक ध्यान की समाधि अवस्था में ज्ञानी सम्पूर्ण विश्व को विचार-संचरण के । रूप में देखता है। वह सगुण और निर्गुण दोनों है।
(ओ) अभावात्मक ध्यान
मैं देह नहीं हूँ। मैं चित्त नहीं हूँ। मैं सच्चिदानन्द हूँ।" उपर्युक्त विचारों का सतत चिन्तन कीजिए। सदा चौबीसों घण्टे यह भावना कीजिए कि आप सत्-चित्-आनन्द स्वरूप है। देह-भाव को नकारिए। अनादि संस्कारों से उत्पन्न देहाध्यास को नष्ट करने के लिए निरन्तर साधना आवश्यक है। देह भावना से यदि आप ऊपर उठ सकें, देह वृत्ति का यदि आप अपने इच्छानुसार त्याग कर सकें, तो आपकी तीन चौथाई साधना पूरी हो गयी। केवल थोड़ी शेष रही। अब केवल परदा हटाना भर, अज्ञान का आवरण नष्ट करना भर शेष रह गया है। वह बड़ी सरलता से किया जा सकता है। चलते-फिरते, काम करते सदा-सर्वदा यह भावना कीजिए कि आप सर्वव्यापी अनन्त ब्रह्मस्वरूप है। यह अत्यन्त आवश्यक है। देह से अपने को अलग करने के लिए विचार, एकाग्रता और प्रयत्न- तीनों एक साथ चलने चाहिए। इस अभावात्मक ध्यान में ज्ञानी शुद्ध, निर्गुण ब्रह्म में ही वास करता है। उसे जगत् की चेतना नहीं रहती ।
६. सगुण तथा निर्गुण ध्यान की तुलना
ईश, प्रश्न, कठ, तापनीय आदि उपनिषदों में निर्गुण ब्रह्मोपासना की प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन है। बादरायण के ब्रह्मसूत्र का एक अध्याय ब्रह्म के गुण की प्रकृति के बारे में व्यवहृत है जिसमें ब्रह्म के ज्ञान, आनन्द आदि भावात्मक गुणों का उल्लेख है तथा साथ ही उसे क्रूर, अवर्ण आदि कह कर उसकी निर्गुणात्मकता का भी वर्णन किया है। उस परमात्मा में दोनों प्रकार के गुण हैं, फिर भी उस ब्रह्म का ध्यान निर्गुण उपासना या निरुपाधिक ब्रह्म का ध्यान कहा जा सकता है। सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना में प्रधान अन्तर इतना ही है कि सगुणोपासना में साधक मानता है कि वे सारे गुण ब्रह्म में वस्तुतः विद्यमान हैं, जब कि निर्गुणोपासना में साधक मानता है कि ब्रह्म की सगुणता या निर्गुणता दोनों उसके अनिवार्य लक्षण नहीं हैं, ये मात्र उसके परिचायक सहायक तत्त्व है। आनन्द आदि गुण अपेक्षित ब्रह्म के लक्षण नहीं हैं, अपितु उसके मूल स्वरूप को पहचानने के माध्यम मात्र हैं। सगुणोपासना में ये सारे गुण ब्रह्म के निज स्वरूप में माने जाते हैं, अतः वे भी ध्यान के अंग ही हैं।
निर्गुण कहने का यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म अभावात्मक तत्त्व है या सत्ता रहित है या शून्य है। उसका अर्थ यही है कि जो गुण यहाँ सीमितता में हैं, वे ब्रह्म में असीमित हैं। इसका अर्थ यह है कि गुण ब्रह्म की अनिवार्य प्रकृति अथवा निज स्वरूप है। अर्थात् ब्रह्म पदार्थ के नाशवान् गुण जैसे वस्त्र के नीले रंग की भाँति नहीं है, बल्कि इसमें सभी श्रेष्ठ गुण, सर्व कल्याण गुण है। ब्रह्म निर्गुण गुणी है। इसी प्रकार निराकार कहने का अर्थ नहीं है कि उसका कोई आकार ही नहीं है। इसका अर्थ है-जगत् के पदार्थों की भाँति उसे सीमित आकार प्राप्त है; किन्तु उसके आकार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनन्त का आप क्या आकार मान सकते हैं? ब्रह्म के सम्बन्ध में कई लोग विचित्र कल्पना करते हैं। वे कहते हैं- "ब्रह्म एक चट्टान है; क्योंकि उसका कोई गुण नहीं है, वह शून्य है।" किन्तु नहीं। यह उनकी बड़ी भूल है। उनमें सद्विचार नहीं है। उनको अनेक प्रकार के सन्देह हैं। उनकी बुद्धि स्थूल है। वे विचार, विवेक, वेदान्त चर्चा, तर्क आदि के योग्य नहीं हैं। उन्होंने निर्भ्रान्त उपनिषदों का, ज्ञान के वास्तविक साधन का, प्रज्ञा के सही स्रोत जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप वर्णन करते हैं, का अध्ययन नहीं किया है। उपनिषद् निर्दोष हैं, क्योंकि वे प्रत्येक विचारक और दार्शनिक की प्रज्ञा को रुचिकर लगती हैं। वे साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं की अनुभूति से मेल खाती है। अतएव उनमें कोई भ्रम नहीं है। उनके प्रमाण प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से परे हैं। ब्रह्म तो परम सूक्ष्म है। वह बाल की नोक के हजारवें भाग से भी सूक्ष्म है। ब्रह्म का ध्यान करने और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यन्त सूक्ष्म, शान्त, शुद्ध, तीक्ष्ण स्वच्छ और एकाग्र बुद्धि आवश्यक है। ये लोग संशय-भावना से पीड़ित हैं। इन्हें बच के यथार्थ स्वरूप तथा उपनिषदों की वैधता पर ही संशय है। इनको निष्काम सेवा द्वारा चित्त को शुद्ध करना चाहिए, उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए, साधन-चतुष्टय को सिद्ध करना चाहिए तथा निरन्तर सत्संग करना चाहिए। तब उनमें ज्ञानोदय होगा और उनकी बुद्धि इन विचारों को ग्रहण करने योग्य होगी। श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन से वे ब्रह्म तक पहुँच सकते हैं। यह उत्तम मार्ग है। अस्तु, ब्रह्म समस्त कल्याण गुणों से परिपूर्ण है। वह ज्योतिर्मय है। वह प्रज्ञानघन है। वह हिमालय से भी बड़ा सघन है, ठोस है। ज्ञान बड़ी-से-बड़ी चट्टान से भी अधिक भारवान् और ठोस है।
सगुणोपासना में भक्त अपने को उपास्य देव से सर्वथा भिन्न मानता है। उपासक प्रभु को परिपूर्ण, अशेष, स्वैच्छिक आत्मार्पण करता है। वह प्रभु की आराधना करता है, प्रणाम करता है, उनको सर्वस्व मानता है और अपने खाने, पहनने, रक्षण तथा अपने अस्तित्व तक के लिए उन पर निर्भर रहता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए वह सदा अपने प्रभु की ओर देखता है। उसके लिए स्वतन्त्र कुछ भी नहीं है। वह प्रभु के हाथों में निमित्त मात्र है। उसके हाथ, पैर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, शरीर- —सब प्रभु के हैं।
ध्यान के प्रकार
भक्त कभी भी प्रभु में लीन होने की कामना नहीं करता। ज्ञान-मार्ग उसे पसन्द नहीं। वह परमेश्वर के सेवक के रूप में अपना अलग अस्तित्व, ईश्वर की आराधना, स्तुति तथा अर्चना करना पसन्द करता है। ज्ञानी की भाँति वह स्वयं शक्कर बनना नहीं चाहता है, बल्कि शक्कर चखना और खाना चाहता है। यह उपासना की पद्धति, संकुचन की पद्धति है। मान लीजिए, एक वर्तुल है और उसके केन्द्र में आप हैं। तब आप उस वर्तुल में सिमटे रहते हैं और उस परिधि के अन्दर सीमित रहते हैं। यह सगुण ध्यान है। भावना प्रधान मनुष्यों के लिए यह पद्धति विशेष अनुकूल है। अधिकांश लोग इसी प्रकार की साधना के योग्य हैं।
निर्गुणोपासना में साधक अपने को ब्रह्मस्वरूप मानता है। शरीर, चित्त, अहंकार आदि मिथ्या उपाधियों को वह मिटा देता है। वह आत्म-निर्भर होता है। वह निर्भीकता पूर्वक अपने अधिकार पर दृढ़ रहता है। वह मनन करता है, तर्क करता है, खोज करता है, विवेक और विचार करता है तथा आत्मा का ही ध्यान करता है। वह शक्कर चखना नहीं चाहता, स्वयं शक्कर की डली बनना चाहता है। वह तल्लीनता चाहता है। वह ब्रह्माकार होना चाहता है। यह निम्न आत्मा के विस्तार की प्रक्रिया है। मान लीजिए, एक वर्तुल है। उसके बीच एक स्थान में कहीं पर आप अवस्थित हैं। साधना करते-करते आपको इतना व्यापक हो जाना है कि आप सारे वृत्त को व्याप्त कर जायें और परिधि को आवृत कर लें। जो व्यक्ति सूक्ष्म ज्ञान प्रधान हैं, सम्यक् प्रज्ञावान्, दृढ़ और शुद्ध विवेकयुक्त, प्रबल संकल्प-शक्ति वाले हैं, यह ध्यान-पद्धति उनके योग्य है। बहुत विरले ही इस ध्यान-मार्ग के सफल अनुयायी हो सकते हैं।
बन्द कमरे में, एकान्त में स्थिर बैठ कर 'अहं ब्रह्मास्मि' का ध्यान करना अपेक्षाकृत सरल है; किन्तु भीड़ में रह कर, शरीर से काम करते समय इस भाव को बनाये रखना बहुत ही कठिन है। दिन में एक घण्टा आप ध्यान करें और अनुभव करें कि "मैं ब्रह्म हूँ" और शेष तेईस घण्टे यही सोचते रहें कि 'मैं शरीर हूँ', तो आपकी साधना नितान्त निरर्थक है और इससे इष्ट-सिद्धि नहीं हो सकती। अतः सदा यह विचार बनाये रखने का प्रयत्न कीजिए कि 'मैं ब्रह्म हूँ। यह बहुत आवश्यक है।
सांसारिक मन का आमूल शोधन करने की, उसमें पूर्ण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। धारणा तथा ध्यान से नव चित्त का निर्माण होता है, विचार की नयी प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। ध्यान-परायण जीवन सांसारिक जीवन से सर्वथा विपरीत है। यह सर्वांगीण और आमूल परिवर्तित जीवन है। इसके लिए दीर्घ काल तकनिष्ठा के साथ सतत और सुदृढ़ अभ्यास से समस्त पुराने विषय संस्कारों को मिटाना होगा और नवीन आध्यात्मिक संस्कारों को अर्जित करना होगा।
७. ध्यान तथा कर्म
मनुष्य में आत्मा, मन और शरीर सन्निहित हैं। आत्मा के दो रूप है अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय बाद वाले को संसार कहते हैं और पूर्व वाले को भगवान्। संसार भी कुछ नहीं है, भगवान् का प्रकट रूप मात्र है। भगवान् गतिमान रूप अर्थात् संसार। उनके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसका सम्बन अस्तित्व है।
आत्मा सर्वव्यापक, सर्वानन्दमय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अनन्त, पूर्ण और शुद्ध है। यह अपनी स्वयं की इच्छा से वे नाम तथा रूप ग्रहण करता है जिसको यह जा कहते हैं। आत्मा में कोई कामना नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई बाह्य विषय नहीं है। इच्छा-शक्ति कहलाती है। यह आत्मा कार्य स्वरूप में है। निर्गुण आत्मा में शक्ति स्ि है। सगुण आत्मा में यह गतिशील है। क्योंकि यह पूर्ण है तथा चूँकि वहाँ कोई ऐसी बान नहीं है जो आत्मा से बाहर हो, इस कारण आत्मा में कोई कामना नहीं होती। कामना आकर्षण होता है जिसमें कि अपूर्णता समाविष्ट होती है। यह इच्छा के अस्तित्व का होना है जो कि भीतर से आकर्षण हेतु निर्धारक होती है। आत्मा चाहती है और समा अस्तित्व में आता है। आत्मा की इच्छा सर्वोपरि रहती है और यह विश्व पर शासन करती है। मन तथा शरीर के सीमित कारकों से एकीकरण के कारण अहंकार, कामन तथा भय के द्वारा मनुष्य इधर-उधर खींचे जाते रहते हैं। सीमितता का विचार अहंकार कहलाता है।
प्रकट तथा अप्रकट सभी अस्तित्वों में ऐक्य का साक्षात्कार ही मानव-जीवन लक्ष्य है। यह ऐक्य पहले ही से अस्तित्वमान है। हम इसे अज्ञानता के कारण भुला हैं। साधना में हमारा सर्वाधिक प्रयत्न इस अज्ञानता के आवरण तथा वह विचार हमने मन और शरीर में बन्द कर रखा है, का उन्मूलन करना है। यह सैद्धान्तिक रु सही है कि यदि एकता का साक्षात्कार करना है, तो विभिन्नता को छोड़ना होगा। हमें विचार कि हम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान हैं आदि को निरन्तर बनाये रखना होगा। कामना के लिए कोई स्थान नहीं होगा; क्योंकि एकता में कोई भावनात्मक आक नहीं है, बल्कि स्थिर, दृढ़, शान्त, अनन्त आनन्द है। मुक्ति पारिभाषिक अयर्थाथत है ।
मोक्ष का अर्थ है-अनन्तता की अवस्था की प्राप्ति। यह पहले ही से अस्तित्वमान है। यह हमारी अनिवार्य प्रकृति है। आपकी प्रकृति में किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है। इस लोक में अथवा परलोक में सन्तति, सम्पत्ति, सुख की सभी कामनाओं का तथा अन्त में मोक्ष की कामना का भी उन्मूलन किया जाना चाहिए तथा सभी कर्म शुद्ध एवं निष्काम भाव से लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट होने चाहिए।
यह साधना- निरन्तर यह अनुभव करने का प्रयत्न कि आप ही सब है—का अभ्यास किया जा सकता है चाहे आप अत्यधिक व्यस्त क्यों न हों। यही गीता की केन्द्रीय शिक्षा है। यह तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है। क्योंकि भगवान् निर्गुण और सगुण दोनी, साकार और निराकार दोनों ही हैं। मन और शरीर को कार्य करने दीजिए। अनुभव करे कि आप उनसे ऊपर है और उन पर नियन्त्रण करने वाले साक्षी है। स्वयं को आधार (मन और शरीर के लिए अवलम्बन) न समझें, यहाँ तक कि जब यह काम करने में लगा हो, तब भी ऐसा न सोचें। हालाँकि प्रारम्भ में ध्यान को आश्रय चाहिए। मात्र एक अतिशय लौह संकल्प वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता है। ध्यान में आधार स्थिर है। इसलिए यह साधना (एकता का प्रयत्न) तुलनात्मक रूप से सरल रहती है। गतिविधियों के मध्य यह प्रयत्न कठिन है। कर्मयोग शुद्ध ज्ञानयोग की अपेक्षा अधिक कठिन है। हमें किसी भी प्रकार से सारे समय अभ्यास करते रखना चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा प्रगति धीरे-धीरे होगी। 'आप ही सब हैं', इस विचार पर कुछ घण्टों का ध्यान तथा दिन के बड़े भाग में मन तथा शरीर के साथ एक रहने का भाव तीव्र अथवा सारभूत प्रगति नहीं ला सकेगा।
विचार के साथ विश्व प्रतीक ॐ को संयुक्त करना और भी उत्तम है। अनादि काल से यह प्रतीक एकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ विधि है ॐ का सारे समय जप करना और इसके अर्थ पर ध्यान करना। लेकिन हमें प्रातःकाल और सायंकाल शुद्ध और सरल ध्यान हेतु कुछ घण्टे अलग रखने ही चाहिए।
अध्याय ६
ध्यान में शारीरिक बाधाएँ
प्रस्तावना
जिस प्रकार पाण्डाल में बिना टिकिट प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए स्वयंसेवक आगे आते हैं, उसी प्रकार शत्रुता, घृणा, वासना, ईर्ष्या, भय, सम्मान, आदर आदि के पूर्व-संस्कार निश्चित रूप ग्रहण कर लेते हैं और साधकों के पथ में बाधा डालते हैं।
भगवद्-साक्षात्कार के पथ में जो बाधा डालते हैं, उन विघ्नों का सम्पूर्ण ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। मात्र तभी साधक उन पर एक-एक करके सरलता से विजय प्राप्त कर सकेगा। जिस प्रकार एक जहाज का चालक पायलेट की सहायता से जहाज को एक खतरनाक समुद्र के किनारे पर बाहर निकाल लाता है, उसी प्रकार एक साधक इन बाधाओं के विस्तृत ज्ञान तथा उन पर विजय प्राप्त करने की विधियों की सहायता से आध्यात्मिकता के समुद्र में मार्ग को स्पष्टतया देख लेता है। इसलिए मैंने विभिन्न बाधाओं तथा उन पर विजय प्राप्त करने हेतु विधियों की अत्यन्त स्पष्ट व्याख्या की है!
साधक जब ध्यान का अभ्यास करता है, तो उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि उसे भगवद्-साक्षात्कार के मार्ग में आने वाली बाधाओं एवं उन पर विजय प्राप्त करने हेतु अनुकूल विधियों का भली प्रकार ज्ञान होगा, तो वह आध्यात्मिक पथ का सरलता से अनुकरण कर सकेगा और बिना किसी अधिक कठिनाई के उन पर विजय प्राप्त कर लेगा।
ध्यान की वास्तविक और भयंकर बाधाएँ मात्र भीतर से ही आती हैं, वे बाहर से नहीं आतीं। मन को उचित प्रकार से प्रशिक्षित कीजिए।
मित्रो! साहसी बने! जब आप मन पर नियन्त्रण करने तथा गहन ध्यान एवं समाधि में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, तो आपको अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।
साधकों से अनुरोध है कि जब उनको मार्ग में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो उन्हें बड़ी ही सावधानीपूर्वक दूर करते रहें।
प्रत्येक साधक को आध्यात्मिक पथ में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बुद्ध, उद्दालक एवं शिखिध्वज ने भी कठिनाइयों का अनुभव किया। आपको इस कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई निराशा नहीं। कोई हताशा नहीं। असफलता सफलता के लिए पायदान का कार्य करती है। अपनी सम्पूर्ण शक्ति और साहस को संचित करें और मार्ग में दुगनी शक्ति तथा ऊर्जा के साथ चल पड़े। अब थोड़ा विश्राम करें।
दृढ़ निश्चयी और लौह संकल्प सम्पन्न व्यक्ति के लिए कोई रोड़ा नहीं आता।
एक ही जन्म में सिद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती। सिद्ध ऋषि गण कई जन्मों के अनेक सत्कर्मों का परिणाम हैं। भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है—“वह योगी जो तत्परतापूर्वक परिश्रम करता है, पाप से शुद्ध हो जाता है और अनेक जन्मों के द्वारा सिद्ध हो जाता है और लक्ष्य तक पहुँच जाता है।” (अध्याय २, श्लोक ४५)
१. निरर्थक भ्रमण
कुछ साधकों को निरर्थक भटकने की आदत होती है। वे एक स्थान पर एक सप्ताह तक भी टिके नहीं रह सकते। इस भटकने की आदत को रोका जाना चाहिए। वे नये स्थान देखना चाहते हैं, नये चेहरे देखना चाहते हैं, नये लोगों से बातें करना चाहते हैं। घूमते हुए पत्थर पर कुछ भी एकत्र नहीं होता। एक साधक को एक स्थान पर कम-से-कम १२ वर्षों (एक तपस्या अवधि) तक निवास करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य दुर्बल है, तो वह गर्मी एवं वर्षा में ६ माह तक एक स्थान पर तथा शीत ऋतु में ६ माह तक दूसरे स्थान पर निवास कर सकता है। शीत ऋतु में वह देहरादून अथवा ऋषिकेश में निवास कर सकता है तथा ग्रीष्म ऋतु में वह बद्रीनाथ अथवा उत्तरकाशी जा सकता है। यदि वह निरन्तर भ्रमण करता रहेगा, तो साधना प्रभावित होगी। जो कठोर साधना करना चाहते हैं, उनको एक ही स्थान पर टिके रहना चाहिए। अत्यधिक भ्रमण से थकान और दुर्बलता उत्पन्न होती हैं।
२. साधना में रुकावट
साधक अपनी साधना के आरम्भ में बहुत अधिक उत्साहित रहता है। वह उत्साह से पूर्ण रहता है। वह साधना में बहुत रुचि लेता है। वह कुछ परिणाम अथवा सिद्धियों की अपेक्षा रखता है। जब उसे वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होते, तो वह निराश हो जाता है तथा अपनी साधना में रुचि खो देता है और अपने प्रयत्नों में ढील दे देता है। तत्पश्चात् वह अपनी साधना को पूर्णतया त्याग देता है। वह साधना की सामर्थ्य में विश्वास खो बैठता है। कभी-कभी मन को एक विशेष प्रकार की साधना में अरुचि हो जाती है, यह एक नयी प्रकार की साधना चाहता है। जिस प्रकार मन भोजन में तथा अन्य चीजों में विभिन्नता चाहता है, उसी प्रकार यह साधना की विधि में भी विभिन्नता चाहता है। यह एक जैसे अभ्यास के प्रति विद्रोह करता है। साधक को जानना चाहिए कि मन को ऐसे अवसरों पर किस प्रकार वश में किया जाये और इसे थोड़ा विश्राम देकर किस प्रकार नियन्त्रित किया जाये। साधना को रोक देना एक बहुत बड़ी भूल है। आध्यात्मिक साधना को किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागा जाना चाहिए। बुरे विचार मानसिक कार्यशाला में प्रवेश करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। यदि साधक अपनी साधना रोक देगा, तो उसका मन माया की कार्यशाला बन जायेगा। किसी भी वस्तु की अपेक्षा न रखें। अपनी नित्य दिनचर्या, तप तथा ध्यान में नियमित और गम्भीर बने। साधना अपनी देखभाल स्वयं कर लेगी।
अपने काम से काम रखिए। परिणाम स्वयं ही प्राप्त होंगे। मुझे भगवान् कृष्ण के शब्दों को दोहराने दीजिए— “आपका काम है कर्म (तप, ध्यान और साधना) करना मात्र, फल की आशा करना नहीं। इसलिए कर्मों का फल आपका लक्ष्य नहीं है, न हो आपको अकर्मण्यता में आसक्त होना है। आपके प्रयत्नों को सगुणी सफलता से विभूषित किया जायेगा। मन के शुद्धिकरण तथा एकाग्रचित्तता की प्राप्ति में बहुत लम्बा समय लगेगा। शान्त और धैर्यवान् बनें। अपनी साधना को नियमित करते रहे।
अपने साथियों के चुनाव में सावधान रहे। अनावश्यक लोग आपकी आस्थ और विश्वास को सरलता से हिला देते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरु तथा जो साधना आप कर रहे हैं, उसमें पूर्ण आस्था रखें। अपनी धारणा को कभी न बदलें। अपनने। साधना को उत्साह के साथ करते रहे। आपकी शीघ्र प्रगति होगी तथा आप आध्यात्मिक सीढ़ी पर एक-एक पायदान चढ़ेंगे और अन्त में लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ।
३. देहाध्यास
जब आप कठोर तप तथा ध्यान हेतु एकान्त-वास पर जायें अथवा जब प्रबल ध्यान के अभ्यास के लिए बन्द कमरे में बैठें, तो दाढ़ी बनाने के लिए अधिक चिन्ता न करें। बालों को बढ़ने दें। ये यान्त्रिक विचार, जैसे दाढ़ी बनाने का विचार, में अत्यधिक विचलन उत्पन्न करते हैं और दैवी विचारों की निरन्तरता में बाधा उत्पन्न
ध्यान में शारीरिक बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। शरीर, दाढ़ी, वस्त्रों आदि के बारे में अधिक विचार न करें। भगवान् अथवा आत्मा के बारे में अधिक विचार करें।
४. रोग
शरीर में रोग दिन में सोने, रात्रि में देर तक जागने, अत्यधिक मैथुन, भीड़ में , मल तथा मूत्र के वेग को रोकने, अपौष्टिक भोजन लेने, अत्यधिक मानसिक घूमने, श्रम तथा नियमित व्यायाम की कमी आदि से होते हैं।
यदि एक योग विद्यार्थी को स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना अथवा अदूरदर्शिता के कारण कोई रोग हो जाता है, तो वह कहता है कि मुझे यह रोग योग के अभ्यास के कारण हुआ है और तब वह अपना अभ्यास बन्द कर देता है। यह योग की प्रथम बाधा है।
यह शरीर भगवद्-साक्षात्कार हेतु एक उपकरण है। यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, तो आप किसी प्रकार का कठोर योगाभ्यास और ध्यान नहीं कर सकेंगे। इस कारण नियमित व्यायाम, आसनों तथा प्राणायाम के अभ्यास, पौष्टिक भोजन, सूर्य स्नान, ताजी हवा, शीतल जल से स्नान आदि के द्वारा इस शरीर को स्वस्थ एवं दृढ़ बनाये रखें।
जिस प्रकार बादल सूर्य को आवृत कर लेते हैं और उसे बाधित करते हैं, इसी प्रकार अस्वस्थता के बादल आपके मार्ग में खड़े हैं, आपको तब भी जप धारणा और ध्यान के अभ्यास को नहीं त्यागना है। अस्वस्थता के छोटे-छोटे बादल शीघ्र ही चले जायेंगे। मन को निर्देश दीजिए— “यह भी शीघ्र बीत जायेगा।” जिस प्रकार आप एक दिन के लिए भी अपने भोजन को त्याग नहीं सकते, उसी प्रकार आपको एक दिन के लिए भी अपनी आध्यात्मिक साधना को नहीं त्यागना चाहिए। मन आपको भ्रमित करने के लिए तथा आपके ध्यान के अभ्यास को रोकने के लिए सदा तैयार रहता है। मन की आवाज न सुनें, आत्मा की आवाज को सुनें।
ध्यान स्वयं ही एक शक्तिवर्धक एवं समस्त रोगों की अचूक औषधि है। यदि आप गम्भीर रूप से बीमार हैं, तो आप बिस्तर में लेटे हुए भी जप और ध्यान कर सकते हैं।
५. बहुत अधिक तर्क करना
कुछ लोग जिनमें बुद्धि विकसित है, उनकी आदत होती है कि वे अनावश्यक आलोचना अथवा विवाद में पड़ जाते हैं। जिनमें तार्किक बुद्धि होती है, वे एक सेकेंड के लिए भी शान्त नहीं बैठ सकते। वे तीखे विवादों हेतु अवसर निर्मित करते हैं। अत्यधिक बहस का अन्त शत्रुता में होता है। निरर्थक विवादों में बहुत-सी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। यदि बुद्धि का प्रयोग आत्म-विचार की सही दिशा में किया जाये, तो वह सहायक है; लेकिन यदि इसका प्रयोग अनावश्यक विवादों में किया जाये, तो बुद्धि एक बाधा है। बुद्धि साधक को अन्तःप्रेरणा की देहली तक ले कर जाती है। बुद्धि भगवान् के अस्तित्व के अनुमान हेतु सहायक है तथा यह आत्म-साक्षात्कार हेतु अनुकूल विधियाँ ढूँढ़ने में सहायता करती है। अन्तःप्रेरणा बुद्धि से परे है; किन्तु बुद्धि की विरोधी नहीं है। अन्तःप्रेरणा सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन है। यहाँ कोई बुद्धि नहीं रहती। बुद्धि भौतिक घरातल के पदार्थों से सम्बद्ध रहती है। जहाँ भी 'क्यों' और 'किसलिए' है, वहाँ बुद्धि है अनुभवातीत विषयों में जो कि बुद्धि से परे हैं, वहाँ बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है।
बुद्धि चिन्तन और तर्क करने में बड़ी सहायक होती है; लेकिन वे लोग जिनमें बुद्धि अत्यधिक विकसित होती है, वे संशयात्मक हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कुमार्गगामी भी हो जाती है। उनका वेदों एवं महात्माओं के उपदेशों में विश्वास नहीं रहता। वे कहते हैं—“हम बुद्धिमान् हैं। हम किसी भी उस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते, जो हमारी बुद्धि को उचित नहीं लगती। हम उपनिषदों में विश्वास नहीं करते। हम उस वस्तु की अस्वीकार करते हैं, जो हमारी बुद्धि के साम्राज्य में नहीं आती। हमारा भगवान् अ सद्गुरुओं में कोई विश्वास नहीं है।" ऐसे बुद्धिवादी लोग एक प्रकार के दुर्बल मनुष्य मात्र हैं। उनको समझाना बड़ा ही कठिन है। उनकी बुद्धि अपवित्र तथा कुमार्गगामी है। ईश्वर के विचार उनकी बुद्धि में प्रवेश नहीं कर सकते। वे किसी प्रकार की आध्यात्मिक साधना नहीं करेंगे। वे कहेंगे"अपने उपनिषदों के ब्रह्म अथवा भक्तों के भगवान् को हमें दिखाओ।" जो संशयात्मक प्रकृति के हैं, वे नष्ट हो जायेंगे। बुद्धि एक सीमित उपकरण है। जीवन की अनेक रहस्यमय समस्याओं की यह व्याख्या नहीं क सकती। जो बुद्धिवाद अथवा तर्कवाद से मुक्त हैं, वे भगवद्-साक्षात्कार के आगे बढ़ सकते हैं।
तर्क करना छोड़ दें। शान्त रहें। अपने भीतर देखें। सभी संशय दूर हो जायेंगे। आपको दैवी ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा। देवी ज्ञान की आन्तरिक पुस्तक के पृष्ठ आपके समक्ष एकदम स्पष्ट होंगे। इसका अभ्यास करें तथा अनुभव करें।
साधकों को मन को विश्राम देने के लिए निरर्थक बातों एवं विचारों में लिप्त नहीं होना चाहिए।
६. वातावरण
असंगत तथा अनुपयुक्त वातावरण एवं बाधाएँ आपके संघर्षों का सामना तेजी से करने में सहायक मात्र होते हैं। आप शीघ्र विकास करेंगे और दृढ़ इच्छा-शक्ति एवं सहन-शक्ति का विकास करेंगे।
७. बुरी संगत
बुरी संगत के प्रभाव बहुत ही भयंकर हैं। साधक को सभी प्रकार की बुरी संगत त्याग देनी चाहिए। बुरी संगत के सम्पर्क से मन बुरे विचारों से पूर्ण हो जाता है। भगवान् और शास्त्रों में जो थोड़ा विश्वास है, वह भी नष्ट हो जाता है। "एक पुरुष उसकी संगत से ही पहचाना जाता है।” “एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं।" ये सभी बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें हैं। ये सभी बिलकुल सत्य हैं। जिस प्रकार एक पौधाघर को प्रारम्भ में गायों आदि से सुरक्षा के लिए अच्छी प्रकार बाड़ आदि से सुरक्षित किया जाता है, उसी प्रकार एक नवाभ्यासी को भी स्वयं को बाहरी प्रभावों से बड़ी ही सावधानीपूर्वक बचाना चाहिए, अन्यथा वह पूर्णतया भ्रमित हो जायेगा। जो झूठ बोलते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, छल करते हैं, धोखा देते हैं, जो लालची हैं, जिनकी भगवान् और शास्त्रों में आस्था नहीं है, जो व्यर्थ की बातों में और चुगलखोरी में लगे रहते हैं, उनकी संगत त्याग देनी चाहिए। स्त्रियों तथा जो स्त्रियों के साथ संयुक्त हैं, उनकी संगत खतरनाक है।
बुरा वातावरण, अश्लील चित्र, अश्लील गीत और उपन्यास जो कि प्रेम, सिनेमा, थियेटर आदि से सम्बन्धित हो, पशुओं के युगल दृश्य, वे शब्द जो मन पर बुरा प्रभाव उत्पन्न करें, संक्षेप में वह सब जो मन में बुरे विचार उत्पन्न करें, वे सभी बुरी संगत के अन्तर्गत आते हैं। साधक गण सामान्यतया शिकायत करते हैं- "हम पिछले पन्द्रह वर्षों से साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी किसी प्रकार की ठोस आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई है।" इसका स्वाभाविक उत्तर है कि उन्होंने बुरी संगत को पूर्णतया नहीं त्यागा है। समाचारपत्र सभी प्रकार के सांसारिक विषयों के बारे में व्यवहत रहते हैं। साधकों को समाचारपत्र पढ़ना पूर्णतया त्याग देना चाहिए। समाचारपत्र-पठन सांसारिक संस्कारों को जगा देता है और मन में वैषयिक उत्तेजना उत्पन्न करता है। मन को बहिर्गामी बनाता है। मन के ऊपर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि यह संसार एक ठोस यथार्थता है और साधक को इन नाम-रूपों के पीछे निहित सत्य को भूलने हेतु विवश करता है।
८. दोष-दृष्टि
यह मनुष्य की घृणित आदत है। यह उसके साथ बुरी तरह चिपकी हुई है। उस साधक का मन सदैव बहिर्गामी होता है जो अन्य लोगों के मामले में ताक-झाँक करता है। यदि आप अपना जितना समय दूसरों के दोष देखने में व्यय करते हैं, उसका थोड़ा-सा भी अंश अपने दोष देखने में खर्च करें, तो आप इस समय के द्वारा एक महान सन्त बन जायेंगे। आप अन्यों के दोषों की चिन्ता क्यों करते हैं। स्वयं को पहले सुधारें। पहले स्वयं को शुद्ध करें। अपने स्वयं के मन की अशुद्धियों को पहले धोयें। स्वयं का पहले पुनर्निर्माण करें। जो स्वयं को उद्यमितापूर्वक आध्यात्मिक साधना में लगाते हैं, उनके पास अन्यों के मामले में दखल देने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं होता। यदि यह दोष ढूँढ़ने वाला स्वभाव नष्ट हो जाये, तो अन्यों की आलोचना करने का समय ही नहीं होगा। चुगलखोरी, कपट करने, षड़यन्त्र रचने आदि में बहुत-सा समय नष्ट हो जाता है। समय अत्यन्त बहुमूल्य है। हमको नहीं मालूम कि कब यमराज हमारी जीवन वापस ले लेंगे। प्रत्येक क्षण का उपयोग दैवी ध्यान में किया जाना चाहिए। संसार को अपने तरीके से काम करने दें। अपने काम से काम रखें। अपनी मानसिक कार्यशाला। को स्वच्छ करें। वह मनुष्य जो दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, वह इस संसार में सर्वाधिक शान्तिपूर्ण मनुष्य है।
९. आत्मस्पष्टीकरण की आदत
यह साधक के लिए खतरनाक आदत है। यह एक पुरानी आदत है। स्वाग्रह अपने पर पूर्ण विश्वास होना, स्वेच्छाचारिता, छल-कपट करना, असत्य बोलना सभी आत्मस्पष्टीकरण के निरन्तर सहयोगी है। जिसने इसका विकास कर लिया, वह कभी स्वयं में सुधार नहीं कर सकता; क्योंकि वह कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता।
वह सदा अपनी तरफ से अनेक प्रकार से स्वयं को सही सिद्ध करने का प्रयास करता रहता है। वह अपनी असत्य बात को सिद्ध करने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलता रहता है और अनन्त झूठ बोलता है। साधक को सदैव अपनी गलतियों, दोषों तथा दुर्बलताओं को उसी समय वहीं पर स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर ही मात्र वह शीघ्र सुधर सकेगा।
१०. आवेग
आवेग ध्यान में बाधा डालते हैं। अवचेतन में छिपे सभी अस्पष्ट आवेगों को बुद्धि और संकल्प के द्वारा नियन्त्रित किया जाना चाहिए।
कामावेग तथा आकांक्षा —दो महान् कारक हैं जो कि ध्यान में बाधा डालते हैं। वे गुरिल्ला युद्ध करते हैं। वे साधकों पर बार-बार आक्रमण करते हैं। वे थोड़े समय के लिए तनु हो गये प्रतीत होते हैं। वे अक्सर पुनर्जीवित हो उठते हैं। कठिन प्रयासों, विवेक, विचार ( आत्मा - अनात्मा के मध्य विवेक शक्ति) द्वारा इनसे मुक्ति पा लेनी चाहिए।
११. अशुद्ध एवं अपौष्टिक भोजन
आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः;
सत्त्वशुद्ध ध्रुव स्मृतिः;
स्मृतिला सर्वग्रन्थिनां विप्रमोक्षः ।
(छान्दोग्य उपनिषद् : ७-२६-२)
"शुद्ध भोजन से शुद्ध प्रकृति होती है, शुद्ध प्रकृति से दृढ़ स्मृति होती है। दृढ़ स्मृति से तीनों ग्रन्थियों (हृदय की) से मुक्ति प्राप्त हो जाती है।'
मन का निर्माण भोजन के सूक्ष्म अंश से हुआ है। यदि भोजन अशुद्ध है, तो मन भी अशुद्ध बन जायेगा। ऐसा ऋषियों और मनोवैज्ञानिकों का कथन है। मन के उत्थान में भोजन की बड़ी भूमिका है। यह मन के ऊपर सीधा प्रभाव डालता है। मांस, मछली, अण्डे, बासी भोजन, कुपोषण युक्त भोजन, प्याज, लहसुन आदि का आध्यात्मिक साधकों के द्वारा परित्याग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वासना और क्रोध को उत्तेजित करते हैं। भोजन को सादा, रेशेदार, हलका, सम्पूर्ण और पौष्टिक होना चाहिए।
मद्य एवं नशीले पदार्थों को कड़ाई से त्याग देना चाहिए। मिर्च-मसाले, मसालेदार भोजन, तीखे पदार्थ, गर्म चीजों तथा खट्टी चीजों एवं मिठाई आदि को त्याग देना चाहिए।
गीता में आप पढ़ेंगे "वह भोजन जो जीवनी-शक्ति, बल, स्वास्थ्य, आनन्द तथा उत्साह में वृद्धि करता है तथा जो स्वादिष्ट और रेशेदार, सारभूत एवं ग्रहणशील होता है, वह सात्त्विक प्रकृति वाले लोगों को पसन्द होता है। एक कामुक व्यक्ति को ऐसा भोजन पसन्द होता है जो गर्म हो तथा जो दर्द, लालच तथा रोग उत्पन्न करता हो। बासी तथा सड़ा हुआ उच्छिष्ट तथा गन्दा भोजन तामसिक मनुष्य को पसन्द होता है" (१८/८, ९ और १०) । साधकों को पेट को अधिक नहीं भरना चाहिए। ९० प्रतिशत रोग भोजन की अनियमितता से उत्पन्न होते है। लोगों को जितना आवश्यक हो, उसमें अधिक भोजन खाने की आदत होती है। हिन्दू माताएँ अपने बच्चों को बहुत अधिक भोजन खिलाती हैं। यह बच्चों की देखभाल करने तथा प्यार करने का तरीका नहीं है। अति-भोजन तन्द्रा तथा तत्काल नींद लाता है। यदि भूख नहीं है, तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए। साधकों के लिए रात्रि भोजन बहुत हलका होना चाहिए। आधा सेर दूध तथा एक या दो केले पर्याप्त हैं। स्वप्नदोष के लिए पेट को अधिक भरना मुख्य कारक है। संन्यासियों तथा साधकों को अपनी भिक्षा उन गृहस्थों से प्राप्त करनी चाहिए जो अपनी आजीविका ईमानदारी के साधनों से कमाते हैं।
१२. साधना में अनियमितता
साक्षात्कार के मार्ग में यह भी महान् बाधा है। जिस प्रकार एक आदमी अपने भोजन को लेने में नियमित है, उसी प्रकार उसे अपनी साधना में भी नियमित होना। चाहिए। उसे प्रातःकाल ३.३० अथवा ४ बजे उठ कर अपना जप और ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति यदि प्रातःकाल तथा रात्रि में नियत समय पर साधना करे, तो उसका ध्यान शीघ्र लग जाता है। ठण्ढ में व्यक्ति चार बार बैठ सकता है। उसे एक ही आसन में, एक ही कमरे में और एक ही आसन पर, एक ही भाव तथा एक ही समय पर ध्यान हेतु बैठना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक नियमित दिनचर्या बना लेनी चाहिए और किसी भी मूल्य पर उस पर टिके रहना चाहिए। मन को ढील देने से सारा कार्यक्रम गड़बड़ा जायेगा। व्यक्ति को नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। उसे ऊर्जा, अथक धैर्य, संकल्प के साथ अथक रूप से आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। तभी उसे सुनिश्चित सफलता प्राप्त होगी। उसे नियत समय पर भोजन लेना चाहिए। उसे नियत समय पर सोना चाहिए और नियत समय पर जागना चाहिए। देखो, सूर्य कैसे निश्चित समय पर उदित होता है और नित्य कार्य करता है।
१३. झटके
अपनी साधना के प्रारम्भ में आपको हाथों, पैरों, वक्ष तथा सम्पूर्ण शरीर में झटके लगेंगे। कभी-कभी ये झटके बड़े ही भयंकर होते हैं। घबरायें नहीं। परेशान न हों। ये कुछ भी नहीं हैं। इनसे कुछ भी नहीं होगा। ये नये प्राणिक प्रभाव अथवा नये नाड़ी-उत्प्रेरण के कारण हुए अचानक पेशीय संकुचन के कारण हैं। स्मरण रखें कि साधना के द्वारा नाड़ियों के शुद्धिकरण के कारण नवीन नाड़ी-तरंगें अब निर्मित हो रही हैं। ये झटके कुछ समय पश्चात् चले जायेंगे। यह ध्यान की क्रिया में प्राणों को धड़ आदि से मस्तिष्क की ओर ले जाने के कारण हैं। डरें नहीं। ध्यान को न बन्द करें। आपको उपर्युक्त सभी स्थितियों से गुजरना होगा। जब आपको ऐसा अनुभव हो, तो जानें कि आप विकास कर रहे हैं। आगे बढ़ें और अध्यवसाय करें। उत्साहित रहें। आपको भीतर से, अन्तर्यामी से, साक्षी, कूटस्थ- प्रत्यग-आत्मा से सहायता प्राप्त होगी। ये सभी नवीन संवेदनाएँ हैं। ध्यान में कुछ लोगों को प्रेरणा होती है तथा वे सुन्दर कविताओं की रचना करते हैं। यदि आपको यह काव्य-प्रेरणा प्राप्त हो, तो उसे लिख लें।
१४. ब्रह्मचर्य की कमी
ब्रह्मचर्य के अभ्यास के बिना कोई आध्यात्मिक प्रगति सम्भव नहीं है। वीर्य एक गत्यात्मक ऊर्जा है। इसे शुद्ध विचारों, जप तथा ध्यान के द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। जो भगवद्-साक्षात्कार करना चाहते हों, उन्हें अटूट ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना चाहिए। गृहस्थ अपनी कमजोरी के कारण संकल्प तोड़ देते हैं। इसलिए उनको आध्यात्मिक पथ में अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता। वे आध्यात्मिक सीढ़ी पर दो कदम ऊपर चढ़ते हैं और ब्रह्मचर्य की कमी के कारण तत्काल भूमि पर आ गिरते हैं। यह बड़ी भूल है। उन्हें अलग-अलग सोना चाहिए। उन्हें गम्भीर होना चाहिए। उन्हें स्थिति की गम्भीरता को स्पष्टतया समझ लेना चाहिए। संकल्प लेना बड़ा ही पवित्र कार्य है। इसे किसी भी मूल्य पर टूटने नहीं देना चाहिए। मनुष्य ही एकमात्र सच्चा अपराधी है। वह नियम और कानून तोड़ता है। स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में अत्यन्त आत्म-संयमी होती हैं, जब कि शास्त्र कहते हैं कि उनमें पुरुषों की अपेक्षा आठ गुना कामुकता होती है।
ब्रह्मचर्य के लाभ और वीर्य के नाश की हानियों का स्मरण रखें। वीर्य का अपव्यय नाड़ी-दौर्बल्य, थकान तथा पूर्णकालिक मृत्यु लाता है। मैथुन का कार्य मन, शरीर एवं इन्द्रियों की शक्ति का नाश कर देता है तथा स्मरण, समझ तथा बुद्धि का नाश कर देता है। यह शरीर भगवद्-साक्षात्कार के लिए बना है। इसका उपयोग उच्च आध्यात्मिक लाभ हेतु अच्छी प्रकार किया जाना चाहिए। मानव जन्म प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। उन ब्रह्मचारियों और सन्तों का स्मरण कीजिए जिन्होंने अमर सम्मान तथा कीर्ति अर्जित की। यदि आप इस वीर्य का संरक्षण करें तथा इसका उपयोग दैवी ध्यान हेतु करें, तो आप भी महानता पा सकते हैं। अब आप रेंग नहीं रहे हैं। आपने खड़े होना और चलना सीख लिया है। आप पुरुष हैं। एक सच्चे पुरुष की भाँति काम करना सीखिए। अपनी पत्नी को भी ब्रह्मचर्य का महत्त्व और महिमा समझायें और इसे स्वयं स्वीकार करें। उसे नित्य स्वाध्याय हेतु धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को दें। उसे एकादशी का उपवास करने एवं किसी भी मन्त्र का २१,६०० बार जप करने को कहें। भगवान् के नाम एवं जप में शरण लें। सभी बाधाएँ दूर हो जायेंगी और आप इस पवित्र संकल्प पर दृढ़ रह सकेंगे।
सन्त पाल ने कहा है—“एक पुरुष के लिए अच्छा है कि वह स्त्री को स्पर्श न करे।" 'भगवान् बुद्ध ने कहा – “एक ज्ञानी पुरुष को विवाहित जीवन से बचना चाहिए, क्योंकि यह जलते हुए कोयलों से भरा गड्ढा है।
१५. ओज
ओज वह आध्यात्मिक ऊर्जा है जो मन में संग्रहित है। श्रेष्ठ विचारों, ध्यान, जप, पूजा तथा प्राणायाम के द्वारा वीर्य ऊर्जा ओज-शक्ति में रूपान्तरित हो जाती है तथा मस्तिष्क में संग्रहित रहती है। यह ऊर्जा दैवी ध्यान तथा आध्यात्मिक कार्यों हेतु प्रयोग की जा सकती है।
क्रोध एवं पेशी ऊर्जा को ओज में रूपान्तरित किया जा सकता है। एक व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में अत्यधिक ओज है, वह प्रचुर मानसिक कार्य कर सकता है। वह अत्यन्त बुद्धिमान् होगा। उसके मुख-मण्डल पर चुम्बकीय आभा-मण्डल एवं उससे नेत्र तेजोमय होगी। वह मात्र कुछ शब्दों को बोल कर ही लोगों को प्रभावित कर सकेगा। उसका छोटा-सा भाषण भी सुनने वालों के मन पर अद्भुत प्रभाव डालने वाला होता है। उसका भाषण आत्मा को झंकृत कर देता है। वह श्रद्धा करने योग्य एवं प्रेरक व्यक्तित्व सम्पन्न होता है। श्री शंकर एक अखण्ड ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपनी ओज-शक्ति से आश्चर्यजनक कार्य किये। उन्होंने दिग्विजय की तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्वानों के साथ अपनी ओज-शक्ति से शास्त्रार्थ किये। एक योगी अखण्ड ब्रह्मचर्य के द्वारा इस दैवी ऊर्जा को एकत्रित करने में अपना ध्यान लगाता है।
१६. यम तथा नियम की कमी
आप समाधि में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि आप ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं हैं। आप गहन ध्यान करने योग्य इसलिए नहीं हैं, क्योंकि आप मन को एकाग्र करने योग्य नहीं हैं। आप धारणा करने योग्य इसलिए नहीं हैं, क्योंकि आप प्रत्याहार का अभ्यास (विषयों से इन्द्रियों को सही प्रकार से नहीं खींच पाते) नहीं कर पाते। आप प्रत्याहार का अभ्यास इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि आपने आसन और प्राणायाम में प्रावीण्यता नहीं प्राप्त की है तथा आप यम और नियम (जो कि योग की नींव हैं) में स्थापित नहीं हैं ।
१७. जिह्वा पेचिश
बहुत अधिक बात करना एक बुरी आदत है जो कि आध्यात्मिक शक्ति घटाती है। यदि एक मनुष्य अत्यधिक बोलता है, तो वह जिह्वा पेचिश से पीड़ित रहता है। शान्त व्यक्ति जिह्वा पेचिश से पीड़ित व्यक्ति के साथ एक मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकते। जिह्वा पेचिश से पीड़ित व्यक्ति ५०० शब्द प्रति सेकेंड तक बोल सकते हैं। उनकी जीभ में एक विद्युत् डायनेमो लगा रहता है। वे बेचैन व्यक्ति हैं। यदि आप उनको एक दिन के लिए एक एकान्त कमरे में बन्द कर दें, तो वे मर जायेंगे। अत्यधिक बात करने में बहुत अधिक ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। बातचीत करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे बचाया जाना चाहिए एवं उसका उपयोग दैवी ध्यान में किया जाना चाहिए। वाक् इन्द्रिय मन को विचलित करती है। एक वाचाल व्यक्ति थोड़े समय के लिए भी शान्ति का स्वप्न नहीं देख सकता। साधक को जब आवश्यक हो, तभी मात्र कुछ शब्द बोलने चाहिए और वह भी मात्र आध्यात्मिक विषयों के बारे में ही। एक वाचाल मनुष्य आध्यात्मिक पथ के लिए एकदम अनुपयुक्त है। नित्य दो घण्टे का मौन का अभ्यास करें, विशेष रूप से भोजन के समय तो मौन होना ही चाहिए। रविवार के दिन २४ घण्टों का पूरा मौन रखें। मौन के समय खूब जप तथा ध्यान करें।
ध्यान के समय जो मौन लिया जाता है, उसे मौन व्रत नहीं माना जाता; क्योंकि फिर तो नींद को भी मौन माना जायेगा। गृहस्थों को मौन ऐसे समय रखना चाहिए जब कि अधिक बात करने का अवसर हो तथा जब मिलने वाले आयें। ऐसा करने पर ही बात करने के आवेग को रोका जा सकेगा। स्त्रियाँ बहुत अधिक बात करती हैं। बेकार की बातों और गपशप से घर में समस्या खड़ी करती है। उन्हें विशेष रूप से मौन रखना चाहिए। आपको मात्र नपे-तुले शब्द ही बोलने चाहिए। अत्यधिक बोलना राजसिक प्रकृति है। मौन के पालन से महान् शान्ति आती है। शनैः-शनैः अभ्यास के द्वारा मौन की अवधि को ३ माह तक बढ़ायें।
१८. गुरु की आवश्यकता
“यदि ये सत्य उस उच्चात्मा को कहे जायें जिसकी भगवान् के प्रति परम भक्ति हो और उसका अपने गुरु के प्रति भी ईश्वर जितना ही प्रेम हो, तभी मात्र वे उसके समक्ष प्रकाशित होंगे।” (श्वेताश्वतरोपनिषद् : ६-२३)
अध्यात्म मार्ग पेचीदा, कठिन तथा प्रवण है। यह अन्धकार से आवृत है। इस पथ में एक ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता होती है जो इस पथ पर पहले चल चुका हो। वे पथ पर प्रकाश डालेंगे तथा साधक की कठिनाइयों को दूर करेंगे। मत्स्येन्द्रनाथ ने निवृत्तिनाथ को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया। निवृत्तिनाथ ने ज्ञानदेव को यह ज्ञान दिया। इसी प्रकार गौडपाद ने गोविन्दपाद को कैवल्य के रहस्य का ज्ञान दिया। गोविन्दपाद ने शंकराचार्य को ज्ञान दिया, शंकराचार्य जी ने सुरेश्वराचार्य को ज्ञान दिया। इस प्रकार परम्परा से गुरु से शिष्य को अनुक्रम से आत्मज्ञान दिया जाता है। अध्यात्म-मार्ग सर्वथा भिन्न मार्ग है। यह स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए प्रबन्ध लिखने जैसा नहीं है। यहाँ प्रत्येक पग पर गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। आजकल नवयुवक साधक अभिमानी, स्वाग्रही तथा उद्धत बन जाते हैं। वे लोग गुरु की आज्ञाओं का पालन करने की चिन्ता नहीं करते। वे गुरु बनाना नहीं चाहते। वे प्रारम्भ से ही स्वतन्त्र रहना चाहते हैं। वे गुरु के चयन में 'नेति नेति' सिद्धान्त तथा भाग-त्याग-लक्षण का प्रयोग करते हैं और कहते हैं: "सर्वं खल्विदं ब्रह्मन गुरुर्न शिष्य: - चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।”
वे सोचते हैं कि वे तुरीयावस्था में हैं, जब कि उन्हें सत् की, आध्यात्मिकता की 'अ आ इ ई' का भी ज्ञान नहीं होता। यह असुरों का दर्शन है। वे स्वेच्छाचारिता अथवा मनमानी को स्वतन्त्रता समझते है। यह एक गम्भीर तथा शोचनीय भूल है। यही कारण है। कि वे उन्नति नहीं करते। वे साधना की क्षमता तथा भगवान् के अस्तित्व में विश्वास खो बैठते हैं। वे कश्मीर से गंगोत्री और गंगोत्री से रामेश्वरम् तक निरुद्देश्य अलमस्त घूमा करते हैं और मार्ग में 'पंचदशी', 'विचारसागर' तथा 'गीता' से उद्धरण दे कर कुछ अनाप-शनाप बकते रहते हैं। वे जीवन्मुक्त होने का ढोंग रचते हैं।
जो गुरु के पथ-प्रदर्शन में बारह वर्ष तक रहता है तथा उनके उपदेशों का निर्विवाद पालन करता है, जो गुरु को परब्रह्म मान कर गम्भीरतापूर्वक उनकी सेवा करता है, उसकी अध्यात्म-पथ पर वास्तविक उन्नति होती है। आध्यात्मिक प्रगति का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। जब तक यह संसार है, तब तक गुरु तथा शास्त्र रहेंगे। यदि आपको कोई आदर्श गुरु नहीं मिलता, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु मान सकते है जो कुछ वर्षों से आत्म-साक्षात्कार के मार्ग पर चल रहा हो, निष्कपट तथा सत्यनिष्ठ हो, निःस्वार्थ हो, जो अभिमान तथा अहंकार से रहित हो, जो सच्चरित्रवान् तथा शास्त्रज्ञ हो। उसके साथ कुछ समय तक रहिए, उसको ध्यान से देखिए। यदि आप उससे सन्तुष्ट हैं, तो उसे अपना गुरु बना लीजिए तथा निष्ठापूर्वक उसके उपदेशों का अनुसरण कीजिए। एक बार उसे गुरु स्वीकार कर लेने के पश्चात् उस पर कभी सन्देह न कीजिए और न उसमें दोष निकालिए। गुरु को बार-बार बदलते न रहिए, आप किंकर्तव्यविमूढ़ हो जायेंगे। आपको परस्पर विरोधी विचार प्राप्त होंगे। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी साधना होती है। यदि आप अपनी साधना-प्रणाली को प्रायः बदलते रहेंगे, तो आपकी कोई प्रगति नहीं होगी। एक ही साधना में लगे रहें, आपका शीघ्र विकास होगा। गुरु, आदर्श, एक ही प्रकार की साधना के प्रति समर्पण तथा सम्पूर्ण हृदय से साधना भगवद्-साक्षात्कार हेतु अनिवार्य योग्यताएँ हैं।
ढोंगी गुरुओं से सावधान! वे आजकल बड़ी संख्या में हैं। वे लोगों को आकृष्ट करने के लिए कुछ चालों आदि का प्रयोग करते हैं। विचार करें कि जिनको अहंकार है, जो शिष्य बनाने तथा धन एकत्र करने के लिए इधर-उधर भ्रमण करते रहते हैं, जो सांसारिक विषयों के बारे में बातें करते हैं, जो असत्य बोलते हैं, जो आत्म-प्रशंसा करते हैं, जो वाचाल हैं, जो स्त्रियों तथा सांसारिक लोगों की संगत में रहते हैं, जो सुविधा भोगी हैं, वे ठग हैं। उनकी मीठी बातों एवं उनके प्रवचनों से भ्रमित न हों।
इस सम्बन्ध में उस व्यक्ति की कहानी सुनाना अनुपयुक्त न होगा जो कि सद्गुरु की खोज में था। उसे अन्त में एक सद्गुरु प्राप्त हो गये। विद्यार्थी ने गुरु से पूछा- ''हे आदरणीय गुरु! मुझे उपदेश दीजिए।” गुरु ने कहा- "तुम कैसा उपदेश चाहते हो?" शिष्य ने कहा- "हे स्वामी! श्रेष्ठ कौन है, शिष्य अथवा गुरु? गुरु ने कहा- गुरु शिष्य से श्रेष्ठ है। " शिष्य ने कहा- "हे गुरु! मुझे गुरु बनाओ, मैं ऐसा चाहता हूँ।" आजकल ऐसे अनेक शिष्य हैं।
१९. अति-भोजन आदि
पेट को अत्यधिक भरना, वह कार्य जो थकान उत्पन्न करे अथवा अत्यधिक श्रम, अत्यधिक बोलना, रात्रि के समय भारी भोजन ग्रहण करना, लोगों के साथ अत्यधिक घुलना-मिलना आदि योग-पथ में बाधाएँ हैं। जब आप अजीर्ण, खट्टी 'डकारें, उल्टी, दस्त अथवा अन्य किसी रोग से पीड़ित होंगे, तो आप ध्यान नहीं कर सकेंगे तथा तब भी ध्यान नहीं कर सकेंगे, जब आप अत्यधिक निराश अथवा थके हुए होंगे।
२०. दुर्बल स्वास्थ्य
बिना साधना या आध्यात्मिक साधना के भगवद्-साक्षात्कार सम्भव नहीं है। आध्यात्मिक साधना उत्तम स्वास्थ्य के बिना सम्भव नहीं है। एक रोगी क्षीण शरीर अभ्यास अथवा संयम के मार्ग में बाधा होता है। साधक को नियमित व्यायाम, आसन, प्राणायाम, मिताहार, भ्रमण, खुली हवा में दौड़ना, कार्य, आहार तथा निद्रा आदि में नियमितता के द्वारा अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए। उसे दवा लेने से यथासम्भव बचना चाहिए। उसे ताजी हवा, पौष्टिक भोजन, शीतल जल से स्नान तथा आहार में समायोजन आदि प्राकृतिक उपचारों से लाभ लेना चाहिए। उसे जीवन की समस्त परिस्थितियों में मन को प्रसन्न रखना चाहिए। प्रसन्नता एक शक्तिशाली मानसिक शक्तिवर्धक है। मन तथा शरीर के मध्य एक अन्तरंग सम्बन्ध है। यदि इनमें से एक प्रसन्न है, तो शरीर भी स्वस्थ होगा। यही कारण है कि आजकल डाक्टर लोग रोगों के उपचार के लिए दिन में तीन बार हँसने के लिए कहते हैं।
कुछ मूर्ख साधक जब वे गम्भीर रूप से बीमार होते हैं, उस समय भी दवा लेने से इन्कार करते हैं। वे कहते हैं-"यह प्रारब्ध है। हमें प्रारब्ध के विपरीत नहीं जाना चाहिए। दवाई लेना भगवान् की इच्छा के विरुद्ध है। शरीर मिथ्या है। यह अनात्मा है। यदि मैं दवाई लूँगा, तो यह देहाध्यास को बढ़ायेगा।" यह मूर्खों का दर्शन है। दवाई लो। पुरुषार्थ करो। परिणामों को प्रारब्ध पर छोड़ दो। यह बुद्धिमानी है। ये मूर्ख लोग अनावश्यक रूप से शरीर को कष्ट देते हैं, रोग को गहरी जड़ें जमाने देते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। वे कोई साधना नहीं कर सकते। वे वेदान्त की गलत धारणा के कारण इस उपकरण को खराब कर लेते हैं। वेदान्त कहता है- "इस शरीर के प्रति कोई मोह न रखें, लेकिन इसे निरन्तर दृढ़ साधना के द्वारा स्वच्छ रखें। यह अमरता की नदी के दूसरे किनारे तक पहुँचने के लिए एक नाव है। यह एक घोड़ा है आपको आपके गन्तव्य तक ले जाने के लिए। इस घोड़े को अच्छी प्रकार भोजन दें, लेकिन 'मेरा पन' छोड़ दें।” मित्र! मुझे बतायें, क्या श्रेष्ठ है? एक रेचक लेना, कुछ दिनों के लिए औषधि लेना, परेशानियों के ऊपर कुछ दिनों में ही रोक लगाना तथा पुनः शीघ्र साधना प्रारम्भ कर देना अथवा रोग की उपेक्षा करना, दवाई नहीं लेना, रोग को बड़ा रूप लेने देना, उपेक्षा के द्वारा एक अथवा दो माह तक कष्ट पाना, रोग को जीर्ण तथा असाध्य बनाना तथा साधना को एक माह के लिए छोड़ देना।
भारत में एक श्रेणी के लोग रसायनों के बारे में बताते हैं। वे सिद्धकल्प ले कर शरीर को दृढ़ तथा स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करते हैं। वे दावा करते हैं कि यह शरीर अमर बनाया जा सकता है। वे कहते हैं- "यह शरीर भगवद्-साक्षात्कार के लिए एक उपकरण है। भगवान् का साक्षात्कार एक स्वस्थ तथा मजबूत शरीर के बिना सम्भव नहीं है। मनुष्य योग में थोड़ी प्रगति करता है और पूर्णता प्राप्त किये बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह अगला जन्म लेता है, योगाभ्यास करता है और पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारा समय जन्म और पुनः मृत्यु में व्यर्थ चला जाता है। यदि शरीर लम्बे समय तक दृढ़ और स्वस्थ रखा जाये, तो मनुष्य एक ही जन्म में भगवद्-साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है।" इस कारण वे नीम का सत्, स्वर्ण, संखिया, गन्धक, पारा आदि से निर्मित कल्पों का सुझाव देते हैं। इन शक्तिवर्धकों के प्रयोग से शरीर दृढ़ बन जाता है और कोई रोग शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। वे शरीर को प्रारम्भ से दृढ़ और स्वस्थ करते हैं।
२१. मित्र
जो मित्र कहलाते हैं, वे आपके वास्तविक शत्रु हैं। आप इस संसार में एक भी निःस्वार्थ मित्र नहीं प्राप्त कर सकते। आपको जिस सच्चे मित्र की आवश्यकता है, वह हैं, आपके हृदय में वास करने वाले भगवान्। जब आप रोल्स रोयल गाड़ी में घूम रहे होंगे, जब आपके पास बहुत सारा धन होगा, तब सांसारिक मित्र आपके पास धन तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए आयेंगे। जब आप विपरीत परिस्थितियों में होंगे, तो कोई भी आपकी सहायता के लिए नहीं आयेगा।
यह संसार लोभ, पाखण्ड, कपट-व्यवहार, चापलूसी, असत्य, धूर्तता और स्वार्थता से पूर्ण है। सावधान रहें! मित्र आपके पास बेकार की बातें करने तथा आपका समय बरबाद करने के लिए आते हैं। उनके पास समय के मूल्य का कोई विचार नहीं होता। वे आपको नीचे गिराने तथा सांसारिक बनाने के लिए आपके पास आते हैं। वे कहेंगे—“मित्र! तुम क्या कर रहे हो? जितना अधिक-से-अधिक सम्भव हो, धन कमाओ। आराम से रहो। खाओ, पियो, शादी करो। हम टाकीज चलेंगे। आज वहाँ एक नयी अमेरीकन फिल्म लगी है। थियेटर में एक सुन्दर अमेरीकन नृत्य होने वाला है। भविष्य के बारे में कौन जानता है? भगवान् कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है? पुनर्जन्म नहीं होता। कोई मुक्ति नहीं है। यह सब पण्डितों की बकवास और कोरी गप्प है। अब आनन्द उठाओ। तुम उपवास क्यों करते हो? इस संसार से परे कुछ नहीं है। सारी साधना और ध्यान बन्द कर दो। तुम अपना समय व्यर्थ गँवा रहे हो।” तुम्हें सांसारिक मित्रों से ऐसी सलाहें मिलेंगी। अपने किसी भी मित्र से बात न करो, चाहे वह कितना भी गम्भीर क्यों न प्रतीत हो। स्वयं को छुपा लो। सदा अकेले रहो। तभी तुम पूर्णतया सुरक्षित रहोगे। उन अमर मित्र पर विश्वास करो, जो तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। वे तुम्हें वह देंगे, जो तुम चाहोगे। एकाग्र मन के साथ उनका मधुर उपदेश सुनो और अनुकरण करो।
२२. सामाजिक प्रकृति
सामाजिक प्रकृति कर्मयोग करने के लिए अच्छी है, किन्तु ध्यानयोग के अभ्यास के लिए बहुत ही बुरी है। यह आपको बाहर खींच ले जायेगी। यह आपके मन को बैचेन बनाती है। यह उन अनेक मित्रों को आमन्त्रित करती है, जो विभिन्न प्रकार से विघ्न डालते हैं।
२३. तन्द्रा, आलस्य और निद्रा
तन्द्रा अर्धनिद्रा अवस्था है। लय का अर्थ भी निद्रा है। आलस्य और तन्द्रा निद्रा के अग्रदूत हैं। ये तीनों साक्षात्कार के पथ में महान् बाधाएँ हैं। निद्रा माया का शक्तिशाली बल है। यह निद्रा-शक्ति है।
लय अथवा मानसिक अकर्मण्यता वह अवस्था है जो गहन निद्रा के समान है। वह वासना के समान बुरी है। लय में मन को जाग्रत रखें।
आप कल्पना करेंगे जैसे कि आप ध्यान कर रहे हैं। मन पलक झपकते ही मूल अज्ञान की पुरानी खाइयों में विश्राम करने हेतु तत्क्षण भाग जायेगा। आपको सन्देह होगा- "क्या मैं सोने चला गया था? अथवा क्या मैंने अभी ध्यान किया? मैं सोचता हूँ कि मैंने थोड़ी झपकी ली थी, क्योंकि मुझे शरीर तथा पलकों में भारीपन का अनुभव हो रहा है।” नींद महान् बाधा है, क्योंकि यह अत्यन्त शक्तिशाली है। हालाँकि साधक बहुत अधिक जागरूक और सावधान रहता है, फिर भी यह उस पर किसी-न-किसी प्रकार से विजय पा ही लेती है। यह आदत बहुत ही दृढ़ है। इस बुरी आदत को दूर करने के लिए समय लगेगा तथा इस हेतु दृढ़ संकल्प-शक्ति की आवश्यकता है।
अर्जुन को ‘गुडाकेश' अथवा 'निद्रा को जीतने वाला' कहते हैं। भगवान् श्री कृष्ण उसे कहते हैं—“हे गुडाकेश!” लक्ष्मण ने भी निद्रा पर विजय प्राप्त की थी। इन दोनों लोगों के अलावा निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अन्य किसी के बारे में हमने नहीं सुना। ऐसे भी लोग है जिन्होंने निद्रा को दो अथवा तीन घण्टे तक सीमित कर दिया है। यहाँ तक कि ज्ञानी और योगी भी दो या तीन घण्टे तक सोते हैं। निद्रा एक मनोवैज्ञानिक विषय है। मस्तिष्क को थोड़े से समय के लिए विश्राम चाहिए, अन्यथा मनुष्य तन्द्रा एवं थकान अनुभव करता है। तब वह न तो काम कर सकता है न ही ध्यान कर सकता है। एक ज्ञानी की निद्रा सांसारिक व्यक्ति से भिन्न होती है। एक ज्ञानी में ब्रह्माभ्यास के शक्तिशाली संस्कार होते हैं। यह कुछ-कुछ ब्रह्मनिष्ठा के समान प्रकृति है। व्यक्ति को उसकी निद्रा कम करने हेतु सावधान रहना चाहिए।
निद्रा को कम करने के लिए इसमें धीरे-धीरे कमी करें। पहले चार माह ११ बजे रात को सोने के लिए जायें और ४ बजे सुबह उठें। पाँच घण्टे की नींद लें। अगले ४ माहों तक १२ बजे रात तक जागें और ३ बजे सुबह उठे। इस प्रकार धीरे-धीरे नींद के घण्टों में कमी करें।
साधक नींद में कमी करके साधना के लिए अधिक समय प्राप्त कर सकते हैं। प्रारम्भ में निद्रा कम करना बड़ा ही कठिन कार्य है। जब आदत बदल जाती है तो यह अन्त में सुखकर हो जाता है।
रात में चावल तथा भारी भोजन का त्याग करें। रात के समय दूध तथा फल के समान हलका भोजन लें। आप प्रातः शीघ्र उठ सकेंगे। ध्यान के समय निद्रा आपको नहीं सतायेगी। जब तमोगुण प्रवेश करेगा तथा जब आप ध्यान प्रारम्भ करेंगे, तो एक घण्टे बाद निद्रा प्रकट होगी।
शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, शलभासन तथा धनुरासन का अभ्यास करें। ध्यान आरम्भ करने से पूर्व थोड़ा प्राणायाम करें। आपको ध्यान के समय निद्रा नहीं सतायेगी।
कभी-कभी ध्यान के समय मन अचानक नींद के लिए अपनी पुरानी लीक में चला जाता है। साधक जब सोते रहते हैं, तब वे सोचते हैं कि वे ध्यान कर रहे थे। चेहरे पर ठण्डे पानी के छींटे मारे तथा ५ या १० मिनट कीर्तन करें। आप सरलता से नींद भगा सकेंगे। यदि नींद आये, तो बत्ती जलाये रखें।
जब ध्यान की आदत हो जायेगी, जब प्रातः ४ बजे की आदत अच्छी तरह स्थापित हो जायेगी, जब आप रात्रि में हल्का भोजन लेंगे, तो नींद आपके ध्यान के समय परेशान नहीं करेगी। जब नींद आप पर विजय पाने का प्रयास करे, तो थोड़ी देर के लिए मन्त्र को जोर-जोर से बोलें। वज्रासन में बैठें।
साधक प्रातः ४-५ बजे तक एक घण्टे ध्यान करते हैं। उसके बाद उन्हें नींद आने लगती है। वे ५ बजे के बाद सोने लग जाते हैं। यह एक सामान्य शिकायत है। ५ बजे १० से २० चक्र प्राणायाम करें। २ मिनट के लिए शीर्षासन करें। आप फिर से ध्यान हेतु ताजा हो जायेंगे। सदैव अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें। पुरानी आदतें बार-बार प्रकट होंगी। इनको अनुकूल साधना, संकल्प-शक्ति, प्रार्थना आदि के द्वारा बार-बार जड़ से दूर करें। शिवरात्रि तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात्रि-जागरण बड़ा ही लाभकारी है। क्रिश्चियन लोग भी क्रिसमस तथा नव-वर्ष की रात्रि पर रात्रि जागरण करते हैं।
ध्यान के समय नींद साधक पर हावी हो जाती है। वह सन्देह करता है कि वह ध्यान कर रहा है या सो रहा है। यदि कोई सच में ध्यान कर रहा होता है, तो उसका शरीर हलका होगा तथा उसका मन उत्साहित होगा। यदि वह सो रहा है, तो शरीर भारी होगा, मन सुस्त होगा और पलकें भारी होंगी।
२४. लौकिक सुख
इत्र, नर्म बिस्तर, उपन्यास-पठन, नाटक, थियेटर, सिनेमा, भद्दा संगीत, नृत्य करना, स्त्रियों का संग, पुष्प, राजसिक भोजन —ये सभी वासना उत्तेजित करते हैं और मन को विचलित करते हैं। अत्यधिक नमक, अत्यधिक मिठाई से अत्यधिक प्यास लगती है तथा ध्यान में बाधा पड़ती है। अत्यधिक बात करना, अत्यधिक चलना, अत्यधिक काम करना और अत्यधिक घुलना-मिलना ध्यान में मन को विचलित करता है।
२५. सम्पत्ति
अर्थ वास्तव में अनर्थ है। सम्पत्ति का अर्जन कष्टदायक है। सम्पत्ति की रक्षा और भी अधिक कष्टदायक है। यदि यह खो जाती है, तो यह असह्य दर्द देती है। आप बिना महान् पाप किये सम्पत्ति का अर्जन और संग्रह नहीं कर सकते हैं। सम्पत्ति अत्यधिक व्याकुलता लाती है। इसलिए धन को त्याग दो।
सेवानिवृत्त अधिकारी गंगा के किनारे निवास करते हैं तथा कुछ वर्षों तक जप और ध्यान का अभ्यास करते हैं, किन्तु वे कोई ठोस प्रगति नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अपनी बड़ी पेंशन का उपयोग स्वयं अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए तथा पुत्रियों के लिए करते हैं। वे इसे दान में प्रयोग नहीं करते। वे हर चीज के लिए धन पर निर्भर हैं।
उन्हें अपना सारा धन दान कर देना चाहिए और ईश्वर पर निर्भर होना चाहिए। उन्हें भिक्षा के ऊपर जीवित रहना चाहिए। उनकी निश्चित ही आध्यात्मिक प्रगति होगी।
अध्याय ७
ध्यान में मानसिक बाधाएँ
१. क्रोध
क्रोध नर्क का द्वार है। यह आत्मज्ञान का नाश कर देता है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह सर्व-उपभोग करने वाला तथा सर्व दूषित करने वाला है। यह शान्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। यह काम का ही रूपान्तरण है। जिस प्रकार दूध दही में बदल जाता है, उसी प्रकार काम-भावना अथवा कामना क्रोध में रूपान्तरित हो जाती है। जब व्यक्ति की कामना की पूर्ति नहीं होती, तो वह क्रोधित हो उठता है। उसका मन भ्रमित हो जाता है। वह अपनी स्मृति तथा सूझ-बूझ खो बैठता है। वह नष्ट हो जाता है। एक मनुष्य जब क्रोधित होता है तो वह जो चाहता है वह कहता है, वह जो चाहता है वह करता है। वह किसी की हत्या भी कर देता है। एक गर्म शब्द झगड़े और शत्रुता में परिणित हो जाता है। उस पर नशा छा जाता है। वह कुछ समय के लिए अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण खो बैठता है। वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। वह क्रोध का शिकार बन गया है। वह क्रोध के चंगुल में है। क्रोध शक्ति अथवा देवी का एक रूप है। चण्डी पाठ में आप पायेंगे :
या देवी सर्वभूतेषु क्रोधरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥
“मैं उस देवी को प्रणाम करता हूँ जो सभी प्राणियों में क्रोध के रूप में स्थित हैं।"
अमर्ष, रोष, प्रकोप, क्रोधोन्माद ये सब तीव्रता के अनुसार क्रोध के ही प्रभेद हैं। यदि एक मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति को सुधारने के लिए, निःस्वार्थ भाव से उसे रोकने और सुधारने के लिए थोड़ा क्रोध करता है, तो यह उचित क्रोध कहलाता है। मान लीजिए कि एक लड़का किसी लड़की को छेड़ता है और यदि वहाँ पास ही खड़ा कोई व्यक्ति इस अपराध के लिए उस पर क्रोध करता है, तो इसे न्यायोचित कहा जायेगा। यह बुरा नहीं है। यह मात्र तभी बुरा है जब यह स्वार्थ अथवा लालच के कारण किया जाता है। कभी-कभी कोई धार्मिक गुरु अपने शिष्य को सुधारने के लिए बाहरी रूप से थोड़ा क्रोध प्रदर्शित करते हैं, यह भी बुरा नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किन्तु उसे भीतर से शान्त होना चाहिए, मात्र बाहर से गर्म और व्यग्र होना चाहिए। उसे अपने अन्तःकरण के भीतर क्रोध को गहरी जड़ें नहीं जमाने देनी चाहिए। इसे समुद्र की लहर की भाँति तत्काल चले जाना चाहिए।
यदि कोई मनुष्य अक्सर छोटी-छोटी चीजों के लिए उत्तेजित हो जाता है, तो यह मानसिक दुर्बलता का निश्चित चिह्न है। क्षमा, धैर्य, विचार, प्रेम, करुणा तथा सेवा की भावना के विकास के द्वारा क्रोध पर विजय पाइए। जब क्रोध नियन्त्रित हो जायेगा, तो यह ऐसी ऊर्जा में रूपान्तरित हो जाता है कि सारे संसार को हिला सकता है। यह ओज में उसी प्रकार रूपान्तरित हो जाता है, जिस प्रकार उष्मा अथवा प्रकाश विद्युत् में रूपान्तरित हो जाती है। ऊर्जा एक अन्य रूप ग्रहण कर लेती है। यदि साधक ने अपने क्रोध पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है, तो उसकी आधी साधना तो पूरी हो गयी । क्रोध आने पर थोड़ा शीतल जल पी लीजिए। इससे मस्तिष्क शीतल होगा तथा उत्तेजित स्नायु शान्त होंगे। ‘ॐ शान्ति' को अनेक बार दोहरायें। धीरे-धीरे एक-एक कर बीस तक गिनें। बीस की गिनती पूरी होने पर क्रोध विलीन हो जायेगा। यदि क्रोध पर नियन्त्रण पाना कठिन प्रतीत हो, तो तुरन्त ही वह स्थान छोड़ दीजिए और आधे घण्टे तक लम्बी सैर कर आइए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। जप कीजिए। ध्यान कीजिए। ध्यान क्रोध तथा अन्य बाधाओं को नष्ट करने के लिए अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है।
मोह से काम का उद्भव होता है। उससे क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से लोभ, अभिमान, ईर्ष्या, घृणा, पूर्वाग्रह, कट्टरता, छिद्रान्वेषण, पिशुनता, मिथ्याचार आदि अन्य सभी दुर्गुण उत्पन्न होते हैं।
मनुष्य कीर्ति, प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा के लिए पिपासु बना रहता है। उपन्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है। साधु अलौकिक सिद्धियाँ चाहता है। संन्यासी विभिन्न देशों में अनेक आश्रम खोलना चाहता है। ये सब लोभ के ही रूप हैं। नापसन्दगी, तिरस्कार, पक्षपात, अवज्ञा, ताना मारना, खिल्ली उड़ाना, उपहास करना, भौंहे चढ़ाना, मुँह बनाना —ये सब घृणा के ही रूप हैं। यदि किसी का पिता किसी व्यक्ति को पसन्द नहीं करता है, तो उसके पुत्र तथा पुत्रियाँ भी उस व्यक्ति से अकारण ही द्वेष करने लगते हैं। द्वेष की शक्ति ही ऐसी है। अँगरेज आयरलैण्ड के निवासी से द्वेष करता है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से द्वेष करता है, मुसलमान हिन्दू से द्वेष करता है, और हिन्दू मुसलमान से । पुत्र अपने पिता के विरुद्ध मुकदमा दायर करता है। पत्नी अपने पति को तलाक दे देती है। ये सब द्वेष के ही प्रकट स्वरूप हैं, जिनके पीछे स्वार्थ भावना छिपी रहती है।
द्वेष के द्वारा द्वेष समाप्त नहीं होता, अपितु यह प्रेम के द्वारा समाप्त हो जाता है। यह विभिन्न दिशाओं में छिपा रहता है। द्वेष को दूर करने के लिए लम्बे समय तक प्रबल अनवरत ध्यान तथा निष्काम सेवा की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में वेदान्त का अभ्यास तथा आत्म-भाव से की गयी सेवा से द्वेष तथा अन्य सभी दुर्गुणों का उन्मूलन किया जा सकता है तथा जीवन की एकता का अद्वैतिक बोध किया जा सकता है।
मैंने अनेक स्थानों पर आपको बतलाया है कि इन दुर्गुणों को पूर्णतया नष्ट करना चाहिए। इन सबको नष्ट करने के अनेक निर्देश भी दिये जा चुके हैं। यदि आपको आध्यात्मिक प्रगति अभीष्ट है, तो आपको इन सबको दूर करना चाहिए। ये सब आत्म-साक्षात्कार के पथ में बाधाएँ हैं। एक निर्भीक आध्यात्मिक सैनिक की भाँति आध्यात्मिक युद्धक्षेत्र में उठ खड़े हों और इन शत्रुओं का संहार करें। एक आध्यात्मिक योद्धा बनें। एक-एक कर सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करें तथा दिव्य महिमा, वैभव, शुचिता और पवित्रता प्रदर्शित करें।
२. चुगलखोरी
यह क्षुद्र बुद्धि सम्पन्न लोगों की घृणित आदत है। लगभग सभी इस भयंकर रोग के शिकार हैं। यह संकीर्ण हृदय शैतान लोगों की जन्मजात आदत बन गयी है। यह तमोगुणी वृत्ति है। संसार की लीला मनुष्य की इस बुरी आदत से चल रही है। यह माया सारे संसार में बेचैनी फैलने वाला शक्तिशाली अस्त्र है। यदि आप कहीं चार लोगों को समूह में बैठे देखें, तो जान लें कि अवश्य ही वहाँ कोई चुगली चल रही होगी। यदि आप चार साधुओं को बातें करते देखें, तो निस्सन्देह समझ लें कि वे किसी-न-किसी व्यक्ति के बारे में चुगली कर रहे होंगे। ये साधु कह रहे होंगे— “क्षेत्र का भोजन बहुत बुरा है। वे स्वामी जी एक बहुत बुरे आदमी हैं।" गृहस्थों की अपेक्षा साधुओं में चुगली की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। यहाँ तक कि शिक्षित संन्यासी तथा गृहस्थ भी इस भयंकर रोग से बचे नहीं है। एक सच्चा साधु सदा अकेला रहता है और ध्यान में लगा रहता है।
निन्दा का मूल कारण अज्ञान अथवा ईर्ष्या है। निन्दा करने वाला झूठे कलंक लगाने, अपयश करने, आक्षेप करने, झूठा अभियोग लगाने आदि के द्वारा उस मनुष्य को नीचे गिराना चाहता है जो कि समृद्धिशाली है। निन्दा करने वाले के पास षड़यन्त्र रचने के सिवा और कोई काम नहीं होता है। वह निन्दा करके ही जिन्दा रहता है। उसे निन्दा करके तथा अनिष्ट करके आनन्द मिलता है। यह उसका स्वभाव है। चुगली करने वाले समाज के लिए खतरा है। वे दुष्ट अपराधी हैं। उन्हें बड़े दण्ड की आवश्यकता है। कपट व्यवहार, कुटिलता, कूटनीति, छल-कपट, बकवाद, ठगी और धूर्तता चुगली के परिजन है। चुगली करने वाले का मन कभी भी शान्त और शान्तिपूर्ण नहीं होता। उसका मन सदैव गलत दिशा में योजना बनाता रहता है। एक साधक को सदा इस दुर्गुण से बच के रहना चाहिए। उसे अकेले घूमना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, अकेले भोजन करना चाहिए तथा अकेले ही ध्यान करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसने ईर्ष्या, निन्दा, घृणा, अहंकार, स्वार्थता आदि को दूर नहीं किया है, यदि वह कहता है कि 'मैं रोज ६ घण्टे ध्यान करता हूँ', तो यह अज्ञानता है। जब तक व्यक्ति इन सभी दुष्प्रवृत्तियों को दूर नहीं करता और मन को शुद्ध नहीं करता, तब तक ६ मिनट तक भी ध्यान लगना सम्भव नहीं है। पहले ६ वर्ष तक निष्काम सेवा द्वारा उसे अपने मन को शुद्ध करना चाहिए।
३. निराशा
नवाभ्यासियों को पूर्व-संस्कारों, सूक्ष्म अस्तित्वों, बुरी आत्माओं के प्रभाव, बुरी संगत, बादल वाले दिन, अपच तथा अधिक भरे पेट से अक्सर ध्यान में हताशा आ जाती है। कारण का उपचार करें। कारण का उन्मूलन करें। निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। तत्काल लम्बी दूरी तक घूमने चले जायें। खुली हवा में दौड़ें। भजन गायें। एक घण्टे तक जोर-जोर से ॐ का उच्चारण करें। समुद्र अथवा नदी के किनारे भ्रमण करें। यदि आप हारमोनियम बजाना जानते हों, तो उसे बजायें। उत्साहजनक विचार रखें और जोर से हँसें। यदि आवश्यक हो, तो विरेचक अथवा पाचक चूर्ण लें।
थोड़े कुम्भक तथा सीतली प्राणायाम करें। सन्तरे का रस, गर्म चाय अथवा एक छोटा कप काफी पियें। 'अवधूतगीता' तथा उपनिषदों के उत्थानकारी अंशों का पठन करें।
जब निराशा आयेगी और आपको कष्ट देगी, तो मन विद्रोह करेगा। इन्द्रियाँ आपकी टाँग खीचेंगीं। गुप्त वासनाएँ मन की सतह पर वेग से आयेंगी तथा आपको सतायेंगी। बहादुर बनें। दृढ़ खड़े रहें। इन झटकों का सामना करें। अपने मन को ठण्ढा रखें। स्वयं को इन बाधाओं से न जोड़ें। अपने जप तथा ध्यान के समय को बढ़ायें। वैराग्य और विवेक को भी बढ़ायें। व्यग्रता से प्रार्थना करें। दूध और फल पर जीवन बितायें। । ये सभी बाधाएँ एक बादल की भाँति चली जायेंगी। सभी परेशानियों के दूर हो जाने पर आप अद्भुत रूप से देदीप्यमान होंगे। आपको विकास का अनुभव होगा। मन, वाणी तथा सभी कार्यों में एक परिवर्तन होगा।
४. संशय
साधक को संशय होने लगता है कि भगवान् का अस्तित्व है या नहीं। वे भगवद्-साक्षात्कार कर पायेंगे या नहीं। आस्था में कमी आध्यात्मिक पथ में भयंकर बाधा है। जब ये सन्देह उत्पन्न होते हैं, तो साधक अपने प्रयासों को ढीला कर देते हैं। माया अत्यन्त शक्तिशाली है। माया रहस्यमय है। यह सन्देह तथा विस्मृति के द्वारा लोगों को भ्रमित करती है। मन माया है। मन लोगों को सन्देह द्वारा भ्रमित करता है। कभी-कभी वह साधना भी त्याग देता है। यह एक गम्भीर भूल है। जब भी किसी साधक पर सन्देह हावी होने लग जाये, तो उसे तत्काल महात्माओं का सत्संग करना चाहिए। उसे उनके साथ उन सन्देहों का निराकरण करना चाहिए। साधारणतया साधक अपनी साधना अनेकों सिद्धियों की शीघ्र प्राप्ति की अपेक्षा के साथ प्रारम्भ करता है। यह परेशानी लगभग सभी मामलों में है। वह सोचता है कि ६ माह में कुण्डलिनी जाग जायेगी तथा उसे दूर-दृष्टि, दूर-श्रवण, विचार-पठन, वायु में उड़ना आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जायेंगी। जब वह उन्हें नहीं प्राप्त कर पाता, तो उसे अरुचि हो जाती है और वह अपनी साधना रोक देता है। वह अनेक काल्पनिक तथा विलक्षण विचारों का पोषण करता है।
मन में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। मन के शुद्धिकरण तथा एकाग्र मन प्राप्त करने में बहुत लम्बा समय लगता है। धारणा अनेक जन्मों की साधना का प्रश्न है। धारणा संसार में सर्वाधिक कठिन वस्तु है। व्यक्ति को कुछ समय अथवा एक या दो माहों अथवा वर्षों की साधना के पश्चात् उससे अरुचि नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि आप थोड़ा-सा भी अभ्यास करेंगे, तो प्रभाव होगा। कुछ भी नहीं व्यर्थ जायेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। आपके पास यदि सूक्ष्म तथा शुद्ध बुद्धि नहीं है, तो आप थोड़े से अभ्यास से प्राप्त होने वाले प्रभावों को नहीं पहचान पायेंगे। आपको सद्गुणी, वैराग्य, धैर्य और सहिष्णुता का उच्चतम स्तर तक विकास करना होगा।
आपका ईश्वर के अस्तित्व तथा आध्यात्मिक साधना की सामर्थ्य में अटल विश्वास होना चाहिए। आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए— मैं अभी इसी जन्म में नहीं, इसी क्षण में भगवद्-साक्षात्कार करूँगा। मैं साक्षात्कार करूँगा या मर जाऊँगा।"
सन्देह तीन प्रकार के है-संशय भावना, असम्भावना तथा विपरीत भावना (गलत भाव कि शरीर आत्मा है और संसार ठोस सच्चाई है)। श्रवण (शास्त्रों को सुनना) संशय भावना का उन्मूलन कर देगा, मनन असम्भावना का उन्मूलन करेगा तथा निदिध्यासन एवं साक्षात्कार विपरीत भावना का उन्मूलन कर देगा।
संशय आत्म-साक्षात्कार के मार्ग में महान् बाधा है। यह आध्यात्मिक प्रगति रोक देता है। इसे सत्संग द्वारा दूर किया जाना चाहिए। इसे धार्मिक पुस्तकों के स्वाध्याय, विचार तथा चिन्तन के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। यह साधक को भटकाने के लिए बार-बार सिर उठाता है। इसे पुनः सिर उठाने से रोकने के लिए दृढ़ निश्चय तथा विवेक बुद्धि पर आधारित अटल विश्वास द्वारा मारा जाना चाहिए।
संशय आपका महान् शत्रु है। सन्देह से मन बेचैन हो जाता है। विचार और ज्ञान के द्वारा सभी सन्देहों को नष्ट कर दें।
सन्देहों की परवाह न करें। सन्देहों का कोई अन्त नहीं है। अपने हृदय को शुद्ध करें। जप, ध्यान आदि शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं में तेजी से लग जायें। नित्य नियमित ध्यान करें। सन्देह अद्भुत तरीके से स्वयं ही स्पष्ट हो जायेंगे। एक महान् गुरु अथवा आन्तरिक शासक आपके साथ हैं। वे आपको प्रकाशित करेंगे तथा आपके सन्देहों को दूर करेंगे।
५. स्वप्न
कुछ साधकों को विभिन्न प्रकार के काल्पनिक स्वप्न परेशान करते हैं। कभी-कभी वहाँ ध्यान और स्वप्न का मिश्रण होता है। चूँकि स्वप्नों का विषय अत्यन्त विशेष तथा अबोध्य है, अतःजब तक कि आप कारण शरीर में स्थित सभी संस्कारों को न पोंछ दें तथा सभी विचारों पर नियन्त्रण न कर लें, स्वप्नों को नियन्त्रित करना बहुत ही कठिन है। जैसे-जैसे आपमें शुद्धता, विवेक, धारणा की वृद्धि होगी, स्वप्न कम हो जायेंगे।
स्वप्नों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप गहन ध्यान में अच्छी तरह स्थापित नहीं है, आपने अभी तक विक्षेपों का उन्मूलन नहीं किया है और आपने निरन्तर प्रबल साधना नहीं की है।
६. बुरे विचार
कल्पना करें कि बुरे विचार आपके मन में १२ घण्टों तक रहते हैं और प्रत्येक तीसरे दिन प्रकट होते हैं। यदि ध्यान एवं धारणा के नित्य अभ्यास के द्वारा आप यह समय १० घण्टे कर सकें तथा सप्ताह में मात्र एक बार प्रकट होने दें, तो यह निश्चित ही प्रगति है। यदि आप अपना अभ्यास निरन्तर करते रहे, तो रुकने की अवधि तथा पुनः प्रकट होना धीरे-धीरे कम हो जायेगा। इसी प्रकार वे धीरे-धीरे अदृश्य हो जायेंगे। पिछले साल से अपनी वर्तमान अवस्था की तुलना करें।
जब बुरे विचार आपके मन में प्रवेश करते हैं, तो आपका मन कभी-कभी काँपता है। यह आध्यात्मिक प्रगति का चिह्न है। आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति पर है। जब आप अपने भूतकाल में किये हुए बुरे कर्मों के बारे में विचार करते हैं, तो आपको बहुत अधिक कष्ट होगा। यह भी आपके आध्यात्मिक उत्थान का द्योतक है। आप उन्हीं कर्मों को पुनः नहीं दोहरायेंगे। आपका मन काँपने लगेगा। जब वही बुरे कर्मों को करने के कुसंस्कार आदत के बल पर वही कार्य करने के लिए आपको उद्यत करेंगे, तो आपका शरीर काँपने लगेगा। पूर्ण शक्ति और उत्कण्ठा से अपना ध्यान करते रहें। सभी बुरे विचार, माया के दुष्ट प्रयत्न स्वयं ही समाप्त हो जायेंगे। आप पूर्ण शुद्धता एवं शान्ति में स्थापित हो जायेंगे।
एक साधक शिकायत करता है—“जैसे ही मैं ध्यान करने लगता हूँ, मेरे अवचेतन मन से अशुद्धियों की पर्तें उठने लगती हैं। कभी-कभी वे इतनी बलशाली और भयंकर होती हैं कि मैं भ्रमित हो जाता हूँ कि उन्हें कैसे रोकूँ। मैं सत्य एवं ब्रह्मचर्य में पूर्ण स्थापित नहीं हूँ। झूठ बोलने तथा वासना की पुरानी आदतें मेरे मन में अभी तक छिपी हुई हैं। काम-वासना मुझे बहुत अधिक सताती है। स्त्री का विचार मेरे मन को उत्तेजित करता है। मेरा मन इतना संवेदनशील है कि मैं उनके बारे में सोचने अथवा सुनने योग्य नहीं हूँ। जैसे ही विचार मन में आता है, वासना के सभी छुपे संस्कार ऊपर उठ जाते हैं। जैसे ही वे विचार मेरे मन में आते हैं, ध्यान तथा सम्पूर्ण दिन की शान्ति भंग हो जाती है। मैं अपने मन को सुझाव देता हूँ कि इनको बहलाओ, इन्हें डराओ; लेकिन कोई लाभ नहीं। मेरा मन विद्रोह करता है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार इस काम-वासना पर नियन्त्रण पाऊँ। चिड़चिड़ाहट, अहंकार, क्रोध, लोभ, घृणा, आदि अभी भी मेरे भीतर छिपे हैं। मैंने अपने मन का अन्वेषण किया है। काम-वासना मोह मेरी सब से बड़ी शत्रु है और यह बड़ी शक्तिशाली भी है। मेरी आपसे विनती है कि आप कृपा करके मुझे सलाह दें कि मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊँ?”
जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, सभी प्रकार के बुरे विचार आपके मन में प्रकट होंगे। जब आप शुद्ध विचारों को लाना चाहते हैं, तो ऐसा ध्यान में क्यों होता है? साधक ध्यान की आध्यात्मिक साधना इसी कारण से छोड़ देते हैं। यदि आप एक बन्दर को भगाना चाहेंगे, तो वह आपके ऊपर हमला कर देगा। इसी प्रकार जब आप उत्तम दैवी विचारों को उठाना चाहते हैं, तो बुरे विचार एवं बुरे संस्कार आप पर उत्तेजना से दुगनी शक्ति से हमला कर देते हैं। जब आप अपने शत्रु को अपने घर से बाहर भगाना चाहते हैं, तो वह उग्रतापूर्वक आपका प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध भी प्रकृति का एक नियम है। पुराने बुरे विचार अड़े रहेंगे और कहेंगे— “हे मनुष्य, निर्दय न बनो! तुमने अनादि काल से हमको अपने मानसिक कारखाने में निवास करने दिया है। हमें यहाँ रहने का अधिकार है। इस समय तक तुम्हारे प्रत्येक बुरे कर्म में हमने सहायता की है। तुम हमें हमारे निवास स्थान से बाहर निकालना क्यों चाहते हो? हम अपना स्थान खाली नहीं करेंगे।" निराश न हो। अपना ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से नित्य करो। ये बुरे विचार तनु हो जायेंगे।
वे सब नष्ट हो जायेंगे। धनात्मक सदैव ऋणात्मक पर विजयी होता है। यह प्रकृति का नियम है। ऋणात्मक बुरे विचार धनात्मक अच्छे विचारों के सामने खड़े नहीं हो सकते। साहस भय पर विजयी होता है। पवित्रता वासना पर विजयी होती है। वास्तविक तथ्य यह है कि जब एक बुरा विचार ध्यान के समय मन की सतह पर आ जाता है, तो आप असहज अनुभव करते हैं। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आप आध्यात्मिकता में विकास कर रहे हैं। उन दिनों आप चैतन्यतापूर्वक सभी बुरे विचारों को आश्रय दे रहे थे। आपने उनका स्वागत किया और उनका पोषण किया। अपनी आध्यात्मिक साधना में दृढ़ रहें। दृढ़ संकल्पित तथा उद्यमशील बनें। आप निश्चय ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि एक आलसी प्रकार का साधक भी यदि निरन्तर २-३ वर्षों तक ध्यानाभ्यास एवं जप का अभ्यास करे, तो उसे भी एक अद्भुत परिवर्तन दिखायी देगा। अब वह अभ्यास नहीं छोड़ सकेगा। यहाँ तक कि यदि वह एक दिन के लिए भी अभ्यास रोक देगा, तो उसे वास्तव में ऐसा अनुभव होगा कि वह उस दिन कुछ खो बैठा- है। उसका मन बेचैन रहेगा।
वासना आपमें छिपी हुई है। आप अति शीघ्र नाराज क्यों हो जाते हैं, आप मुझसे इसका कारण पूछ सकते हैं। क्रोध और कुछ नहीं मात्र वासना का रूपान्तरण है। जब कामना पूर्ण नहीं होती, तो यह क्रोध का रूप लेती है। क्रोध का वास्तविक कारण है असन्तुष्ट वासना। जब आप अपने नौकर को उसकी गलतियाँ बतलाते हैं, तो यह स्वयं ही क्रोध के रूप में अभिव्यक्त होती है। यह इसके अभिव्यक्तिकरण के लिए अप्रत्यक्ष कारण अथवा बाह्य उत्प्रेरक है। राग-द्वेष की तरंगें पूर्णतया बाहर नहीं निकाली गयी हैं। वे मात्र कुछ मात्रा में तनु हो पायी हैं। इन्द्रियाँ अभी भी उपद्रवी हैं। वे कुछ अंशों में वशीकृत हुई हैं। वहाँ वासनाओं तथा तृष्णाओं के गुप्त प्रभाव है। इन्द्रियों की बाहर जाने वाली प्रवृत्तियाँ अभी भी पूर्णतया रोकी नहीं गयी हैं। आप प्रत्याहार में स्थापित नहीं हैं। वृत्तियाँ अब भी शक्तिशाली हैं। आपमें दृढ़ तथा स्थिर विवेक अथवा वैराग्य नहीं है। भगवान् के प्रति तीव्र अभिलाषा नहीं जागी है। रजोगुण तथा तमोगुण अभी भी उपद्रव मचा रहे हैं। आपमें मात्र सत्त्व की मात्रा में थोड़ी-सी वृद्धि हुई है। बुरी वृत्तियाँ तनु नहीं हुई हैं। वे अभी भी शक्तिशाली हैं। सद्गुणों का उचित मात्रा में अर्जन नहीं किया गया है। यही कारण है कि आपको पूर्ण धारणा प्राप्त नहीं हुई। सर्वप्रथम मन का शुद्धिकरण करें। धारणा स्वयं ही आयेगी।
ध्यान के प्रारम्भ में सांसारिक विचार आपको बहुत अधिक परेशान करेंगे। यदि आप ध्यान में नियमित हैं, तो ये विचार स्वयं ही मृत हो जायेंगे। ध्यान इन विचारों को जलाने के लिए एक अग्नि है। सभी सांसारिक विचारों को बाहर भगाने का प्रयत्न न करें। ध्यान के विषय से सम्बन्धित विचारों का स्वागत करें।
अपने मन को सदा अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखें। जागरूक बनें। सतर्क रहें। उत्तेजना, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा तथा वासना की तरंगों को मन में न उठने दें। ये गहन तरंगें ध्यान, शान्ति तथा ज्ञान की शत्रु हैं। इन्हें उत्कृष्ट तथा दैवी विचारों के प्रवेश द्वारा दबायें। उत्तम विचारों को उत्पन्न करके तथा किसी भी मन्त्र अथवा भगवान् के नाम का जप करके, भगवान् के किसी भी रूप का विचार करते हुए भगवान् के नाम का गायन करके, उत्तम कार्य करने के द्वारा तथा बुरे विचारों से उत्पन्न होने वाले कष्टों के बारे में विचार मन में बनाये रख कर, उठने वाले बुरे विचारों को नष्ट किया जा सकता है। जब आप शुद्धता की अवस्था प्राप्त कर लेंगे, तो कोई भी बुरा विचार आपके मन में नहीं उठेगा। जिस प्रकार एक शत्रु अथवा अनधिकृत प्रवेश करने वाले को गेट पर ही रोकना आसान है, उसी प्रकार किसी भी बुरे विचार को इसके जन्मते ही वश में करना आसान रहता है। कलिका को कुचल दें। इसे गहरी जड़ें न जमाने दें।
आपके विचार नियन्त्रण के अपने अभ्यास के प्रारम्भ में आपको अत्यन्त कठिनाई का अनुभव होगा। आपको उनके साथ कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। वे अपने अस्तित्व के लिए अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न करेंगे। वे कहेंगे-"हमें मन के इस स्थान में रहने का अधिकार है। हमें अनादि काल से इस क्षेत्र को अधिग्रहित करने का एकाधिकार है। हम अपना राज्य क्यों खाली करें? हम अन्त तक अपने जन्म सिद्ध अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे।" वे आपके ऊपर बड़ी तीव्रता से आक्रमण करेंगे। जब आप ध्यान हेतु बैठेंगे, तो सभी प्रकार के बुरे विचार आपके भीतर से उठेंगे। यदि आप उन्हें दबाने का प्रयत्न करेंगे, तो वे आपके ऊपर दुगनी शक्ति से आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन धनात्मक सदैव ऋणात्मक पर विजयी होता है। जिस प्रकार अँधेरा सूर्य के सामने नहीं खड़ा रह सकता, इसी प्रकार ये सभी गहन, नकारात्मक विचार, ये अनधिकृत प्रवेश करने वाले शान्ति के अदृश्य शत्रु उत्कृष्ट विचारों के समक्ष नहीं खड़े रह सकते। वे स्वयं ही मृत हो जायेंगे।
जब आप नित्य कार्यों में बहुत व्यस्त होते हैं, तो आप किसी भी अशुद्ध अथवा शुद्ध विचार को आश्रय नहीं देते। लेकिन जब आप विश्राम करते हैं, तो मन को खाली छोड़ देते हैं। इस समय अशुद्ध विचार छलपूर्वक भीतर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। आपको तब सावधान रहना चाहिए, जब मन ढीला छोड़ा हो।
७. मिथ्या तुष्टि
साधक को अपनी साधना के समय कुछ अनुभव होते हैं। वह ऋषियों, महात्माओं के तथा कई प्रकार के सूक्ष्म अस्तित्वों आदि के अद्भुत दृश्यों को देखता है। अनेक मधुर अनाहत ध्वनियों को सुनता है। उसे दिव्य गन्ध आती है। वह विचार- पठन, भविष्य-कथन आदि की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। साधक अब मूर्खतापूर्ण कल्पना करता है कि वह सर्वोच्च लक्ष्य पर पहुँच गया है और वह साधना बन्द कर देता है। यह एक भयंकर भूल है। वह मिथ्या तुष्टि प्राप्त कर लेता है। ये सभी शुभ संकेत हैं जो थोड़ी-सी शुद्धता तथा धारणा के कारण प्रकट होते हैं। ये सभी प्रोत्साहन हैं जो आगे की प्रगति तथा प्रबल साधना हेतु भगवान् के द्वारा प्रेरित एक प्रकार का उत्प्रेरण है। साधक को इन अनुभवों से दृढ़ विश्वास और बल प्राप्त होता है।
८. भय
यह भगवद्-साक्षात्कार के मार्ग में बड़ी महान् बाधा है। एक भीरु साधक आध्यात्मिक पथ हेतु बिलकुल अनुपयुक्त है। वह एक हजार जन्मों में भी साक्षात्कार का स्वप्न नहीं देख सकता। यदि कोई अमरता चाहता है, तो उसे अपना जीवन भी दाँव पर लगा देना चाहिए। आत्म-त्याग के बिना आध्यात्मिक सम्पत्ति अर्जित नहीं की जा सकती। एक निर्भय डाकू जिसके भीतर देहाध्यास न हो, वह भगवद्-साक्षात्कार हेतु अधिकारी है। मात्र उसकी प्रकृति परिवर्तित करने की आवश्यकता है। भय एक काल्पनिक अनस्तित्व है। यह ठोस रूप ग्रहण कर लेता है और साधकों को अनेक प्रकार से परेशान करता है। यदि कोई भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वह सफलता के पथ पर है। वह लक्ष्य तक पहुँच गया है। तान्त्रिक साधना साधकों को निर्भय बनाती है। यह इस साधना का एक बड़ा लाभ है, क्योंकि उनको श्मशान घाट में मृत शरीर के ऊपर बैठ कर मध्य रात्रि में अभ्यास करना होता है। इस प्रकार की साधना विद्यार्थी को साहसी बनाती है। भय अनेक रूप ग्रहण करता है जैसे मृत्यु का भय, रोग का भय, बिच्छू के काटने का भय, अकेलेपन का भय, साथ का भय, किसी चीज के खो जाने का भय तथा लोगों की आलोचना का भय कि लोग क्या कहेंगे।
कुछ लोग जंगल में शेर से भी नहीं डरते, कुछ युद्ध में गोलियों से भी नहीं घबराते; लेकिन वे लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचना से बहुत घबराते हैं। लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचना का भय साधक की आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में खड़ा रहता है। चाहे उसे यातना दी जाये अथवा उसे तोप से उड़ा दिया जा रहा हो, उसे अपने सिद्धान्तों तथा धारणाओं पर दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा होने पर ही मात्र वह विकास एवं साक्षात्कार कर सकेगा। सभी साधकों को इस भयंकर रोग भय से पीड़ित होना पड़ता है। सभी प्रकार के भयों का आत्म-चिन्तन, विचार, भक्ति तथा विपरीत गुण साहस के अर्जन द्वारा उन्मूलन किया जाना चाहिए। धनात्मक सदैव ऋणात्मक पर विजयी होता है। साहस सदैव भय एवं भीरुता पर विजयी होता है।
मन के रहस्यमय सूक्ष्म कार्यों को समझने में मुझे वर्षों लग गये। मन कल्पना-शक्ति के द्वारा विध्वंस करता है। अनेक प्रकार के काल्पनिक भय, अतिशयोक्ति, षड़यन्त्र-रचना, मानसिक नाटक, हवाई किले बनाना आदि सभी कल्पना-शक्ति के कारण हैं। यहाँ तक कि एक पूर्ण स्वस्थ मनुष्य को भी मन की कल्पना-शक्ति के कारण किसी प्रकार का काल्पनिक रोग होता है। एक मनुष्य में थोड़ी दुर्बलता अथवा दोष हो सकता है; किन्तु जब वह आपका शत्रु बन जाता है, तो आप उसकी दुर्बलता तथा दोष को तत्काल बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं। यहाँ तक कि आप उस पर अन्य अनेक दुर्बलताओं तथा दोषों को अध्यारोपित कर देते हैं। यह कल्पना-शक्ति के कारण होता है। काल्पनिक भय के कारण बहुत-सी ऊर्जा का अपव्यय हो जाता है।
९. मन की अस्थिरता
यह ध्यान की महानू बाधा है। हल्का सात्त्विक आहार तथा प्राणायाम का अभ्यास मन की इस स्थिति का उन्मूलन करता है। पेट को अधिक न भरें। अपने बरामदे में आधा घण्टे तक इधर-उधर टहलें। जैसे ही आप एक दृढ़ संकल्प करें, आपको किसी भी मूल्य पर इसका पालन करना है। यह मन की अस्थिरता को दूर करेगा तथा आपकी संकल्प शक्ति का विकास करेगा।
१०. ध्यान में पाँच बाधाएँ
ध्यान की पाँच बाधाएँ हैं—विषयों की कामना, दुर्भावना, सुस्ती और ढीलापन तथा उद्विग्नता। इनको दूर किया जाना चाहिए; क्योंकि जब तक इन्हें दूर नहीं किया जायेगा, ध्यान नहीं हो पायेगा। जो मन विषयों की कामना के कारण अनेक विषयों के पीछे भागता है, वह विषयों की कामना के वशीभूत होने के कारण एक विषय अथवा प्राणी पर केन्द्रित नहीं हो सकेगा। यह विषयी तत्त्व पर लगा होने के कारण ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मन जो कि दुर्भावना के कारण किसी विषय से सम्बद्ध है, वह तत्काल इसे नहीं छोड़ेगा। मन जो कि सुस्ती और ढीलेपन द्वारा वशीभूत रहता है, वह स्थूल होता है। यह शान्त नहीं होता, बल्कि झटके खाता रहता है। व्याकुलता का आक्रमण होने पर यह उस मार्ग पर नहीं जाता जो कि ध्यान तथा समाधि की प्राप्ति हेतु जाता है।
११. पुराने कुसंस्कारों का दबाव
जब साधक बुरे संस्कारों के उन्मूलन हेतु प्रबल साधना करता है, तो वे क्रोध तथा दुगने बल से उसे बाँधने का प्रयत्न करते हैं। वे रूप ले कर उसके सामने रोड़ों की भाँति आते हैं। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, लज्जा का भाव, आदर, सम्मान, भय आदि के पुराने संस्कार बड़ा भयंकर रूप ले लेते हैं। संस्कार काल्पनिक अनस्तित्व नहीं है। वे जब अवसर मिलता है, तो वास्तविकता में बदल जाते हैं। साधक को हताश नहीं होना चाहिए। कुछ समय बाद उनका बल क्षीण हो जायेगा और वे स्वयं ही मर जायेंगे। जिस प्रकार एक बत्ती अन्तिम बार बहुत तीव्रता से जलती है, उसी प्रकार ये पुराने संस्कार बाहर निकाले जाने के पूर्व अपने दाँत और बल दिखायेंगे। साधकों को अनावश्यक रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्कर्म, सत्संग तथा सात्त्विक गुणों के अर्जन करने के द्वारा आध्यात्मिक संस्कारों के बल की गति को बढ़ाना चाहिए। नवीन आध्यात्मिक संस्कार पुराने कुसंस्कारों को उदासीन कर देंगे। उसे अपनी साधना में तत्पर रहना चाहिए। उसे अपनी आध्यात्मिक साधना में लगे रहना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है।
जब आप सन्ध्या के समय पुनः ध्यान हेतु बैठेंगे, तो दिन-भर में जो संस्कार आपने एकत्र किये हैं, उन्हें पोंछने तथा एकाग्र मन को पुनः प्राप्त करने हेतु आपको बड़ा कड़ा संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष से सिरदर्द होने लगेगा। वह प्राण जो विभिन्न गलियों से भीतर की ओर जाता है तथा ध्यान के समय सूक्ष्म होता है, उसे सांसारिक गतिविधियों में नयी और भिन्न दिशाओं में जाना पड़ता है। यह काम के समय बहुत स्थूल हो जाता है। ध्यान के समय प्राण सिर की ओर ऊपर ले जाया जाता है।
१२. उदासी तथा नैराश्य
जिस प्रकार बादल सूर्य को ढाँक लेते हैं और उसे बाधित करते हैं, उसी प्रकार उदासी तथा निराशा आपकी साधना के मार्ग में बाधा डालती हैं। तब भी आपको अपने जप, धारणा तथा ध्यान के अभ्यास को नहीं छोड़ना है। ये निराशा के बादल शीघ्र चले जायेंगे। मन को सुझाव दें— “यह भी गुजर जायेगा।”
१३. लालच
सबसे पहले काम आता है। उसके बाद क्रोध आता है। इसके बाद लोभ आता है। उसके बाद मोह आता है। काम अत्यन्त शक्तिशाली है। इसलिए इसे प्रमुखता दी जाती है। काम और क्रोध के मध्य अन्तरंग सम्बन्ध है। इसी प्रकार लोभ तथा मोह के साथ निकट सम्बन्ध है। एक लोभी मनुष्य को उसके धन के प्रति बड़ा मोह होता है। उसका मन सदैव तिजोरी तथा कमर पर बँधे चाभियों के गुच्छे पर रहता है। धन उसका रक्त और जीवन है। वह धन एकत्र करने के लिए जीवित रहता है। वह अपने धन का रखवाला मात्र है। उसका आनन्द उठाने वाला उसका अतिव्ययी पुत्र है। धन एकत्र करने वाले हमारे मित्र लोभ के अच्छे औजार हैं। उसने उनके मनों में गहरी पकड़ कर ली है। वे वर्तमान काल के निर्दय महाजन हैं। वे गरीब लोगों से अत्यधिक ब्याज (२५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत तथा १०० प्रतिशत ब्याज) ले कर उनका खून चूसते हैं। निर्दय हृदय लोग क्षेत्र खोलने, मन्दिर बनाने आदि जैसे कार्य करके ऐसा दिखावा करते हैं कि वे बड़े दानी हैं।
ऐसे कार्य उनके घृणित पापों तथा क्रूर कर्मों को निष्प्रभावी नहीं कर सकते। अनेक गरीब परिवार इन लोगों के द्वारा भ्रमित किये जाते हैं। वे नहीं सोचते कि जिन बंगलों तथा कोठियों में वे निवास कर रहे हैं, वे इन गरीब आदमियों के खून से बने हैं। लालच ने उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है और उन्हें एकदम अन्धा बना दिया है। उनके पास नेत्र हैं, पर वे देखते नहीं हैं। लोभ हमेशा मन को बैचेन बना देता है। एक मनुष्य जिसके पास १ लाख रुपये हैं, वह १० लाख रुपये प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक अरबपति खरबपति बनने की योजना बनाता है। लोभ कभी सन्तुष्ट होने वाला नहीं है। इसका कोई अन्त नहीं है। लोभ अनेक सूक्ष्म रूप ग्रहण कर लेता है जैसे कि एक मनुष्य नाम, यश तथा प्रशंसा को तृषित रहता है। यह लोभ है। एक उप न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है। एक तृतीय श्रेणी न्यायाधीश प्रथम श्रेणी न्यायाधीश बनना चाहता है। एक साधु विभिन्न केन्द्रों में कई आश्रम बनाना चाहता है। यह भी लोभ है। एक लोभी मनुष्य आध्यात्मिक पथ हेतु पूर्ण अयोग्य है। सभी प्रकार के लोभ को विचार, भक्ति, ध्यान, सन्तोष, जप, सच्चाई, ईमानदारी तथा अरुचि के द्वारा नष्ट कर दें और शान्ति का उपभोग करें।
१४. घृणा
यह साधक की मारक शत्रु है। यह एक बिना रीढ़ की शत्रु है। यह जीव की पुरानी संगी है। घृणा, अनादर, पूर्वाग्रह, उपहास करना, चिढ़ाना, तिरस्कार करना, क्रोध करना तथा मुँह चिढ़ाना —ये सभी घृणा के रूप हैं। घृणा बार-बार भड़कती है। यह काम तथा लोभ की भाँति कभी सन्तुष्ट नहीं होती। यह कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से विलीन हो जाती है और पुनः दुगनी शक्ति से फूट पड़ती है। यदि पिता किसी व्यक्ति से घृणा करता है तो उसके पुत्र और पुत्रियाँ भी बिना किसी कारण से उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं, चाहे उस व्यक्ति ने उनके साथ कुछ भी बुरा या गलत न किया हो, तो भी वे उससे घृणा करते हैं। घृणा का ऐसा बल है। यदि किसी को उस व्यक्ति का ध्यान आता है, जिसने ४० वर्ष पूर्व उसके साथ कोई गहरा आघात किया हो, तो तत्काल घृणा उसके मन में उठती है और घृणा या शत्रुता के स्पष्ट चिह्न उसके चेहरे पर दिखायी देते हैं।
घृणा घृणा वृत्ति की पुनरावृत्ति का विकास करती है। घृणा घृणा से नहीं रुकती, मात्र प्रेम से रुकती है। घृणा के लिए लम्बे समय तक प्रबल उपचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी शाखाएँ अवचेतन मन में विभिन्न दिशाओं में विभाजित हैं। यह विभिन्न कोनों में दुबकी बैठी है। ध्यान के साथ निरन्तर निष्काम सेवा १२ वर्षों तक आवश्यक है। एक अँग्रेज आदमी आयरलैंड निवासी से घृणा करता है। आयरलैंड वाला अँग्रेज से घृणा करता है। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से घृणा करता है और प्रोटेस्टेंट कैथोलिक से घृणा करता है। यह धार्मिक घृणा है। साम्प्रदायिक घृणा भी होती है। एक व्यक्ति बिना किसी कारण के पहली दृष्टि में ही किसी व्यक्ति से घृणा करता है। यह स्वाभाविक है। इस संसार में सांसारिक लोगों के भीतर शुद्ध प्रेम अनजाना है। स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ तथा वासना घृणा के अनुचर है। कलियुग में घृणा का बल बढ़ गया है।
एक पुत्र अपने पिता से घृणा करता है और उसे न्यायालय में घसीटता है। पत्नी अपने पति को तलाक दे देती है। यह आजकल भारत में भी आ गया है। कुछ समय बाद भारत में भी तलाक न्यायालय स्थापित हो जायेंगे। हिंदू स्त्रियों का पतिव्रता धर्म कहाँ चला गया है? क्या यह भारत की भूमि से चला गया है? भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार समझौता नहीं है। यहाँ पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है, दोनों आकाश में अरुन्धती तारे को देखते हैं और अग्नि के समक्ष पवित्र शपथ लेते हैं। पति कहता है—“मैं राम की भाँति पवित्र रहूँगा और तुम्हारे साथ शान्तिपूर्वक रहूँगा और स्वस्थ बुद्धिमान् सन्तान उत्पन्न करूँगा। मैं मरते दम तक तुमसे प्रेम करूँगा। मैं किसी अन्य स्त्री का मुख नहीं देखूँगा। मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार रहूँगा। मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊँगा।” पत्नी कहती है- “मैं आपके लिए जैसे कृष्ण के लिए राधा थी और राम के लिए सीता थी, उस प्रकार रहूँगी। मैं अपने जीवन के अन्त तक लगनपूर्वक आपकी सेवा करूँगी। आप मेरा जीवन हैं। आप मेरे प्राणवल्लभ हैं। मैं आपकी सेवा ईश्वर की भाँति करते हुए भगवद्-साक्षात्कार प्राप्त कर लूँगी।” आजकल की सम्बन्धों की भयंकर स्थिति की ओर देखिए । यह शोकजनक स्थिति आधुनिक सभ्यता तथा आधुनिक शिक्षा के कारण हुई है। पतिव्रता धर्म जाने कहाँ चला गया है। स्त्रियाँ स्वतन्त्र बन गयी हैं। वे पति को छोड़ कर जो चाहती हैं, वह करती हैं। पति-पत्नी के माउंट रोड तथा मरीना बीच पर हाथ में हाथ पकड़े रहने तथा पति के कन्धों पर हाथ रखे रहने से संस्कृति नहीं जीवित रह सकती। यह सच्ची स्वतन्त्रता नहीं है। यह तुच्छ अनुकरण है। यह अन्धानुकरण की आदत हिन्दू स्त्रियों को नारीत्वहीन कर देगी और स्त्रियोचित शोभा एवं पवित्रता जो उनका गुण है और जो उन्हें धारण करना चाहिए, को नष्ट कर देगी।
शुद्ध निःस्वार्थ प्रेम का अर्जन किया जाना चाहिए। व्यक्ति को ईश्वर का भय होना चाहिए। सोलोमन कहता है-"भगवान् का भय ज्ञान का आरम्भ है। आत्म-भाव से सेवा घृणा का पूर्णतया उन्मूलन करती है और व्यक्ति के जीवन में अद्वैतिक साक्षात्कार लाती है। निष्काम सेवा से घृणा, पूर्वाग्रह, अनादर आदि का पूर्णतया उन्मूलन किया जाता है और यह सभी प्रकार की घृणा का उन्मूलन कर देता है। सभी प्राणियों में एक ही आत्मा छिपी हुई है। आप दूसरों पर क्रोध क्यों करते हैं? आप दूसरों का अनादर क्यों करते हैं? आप विभाजित और पृथक क्यों होते हैं? जीवन और चेतना के मिलन का साक्षात्कार कीजिए। सर्वत्र आत्मा का अनुभव कीजिए। आनन्द का उपभोग कीजिए तथा सर्वत्र प्रेम और शान्ति का विकिरण कीजिए।
१५. अधैर्य
जब आप ध्यान हेतु आसन में बैठते हैं, तो आप पैरों में दर्द के कारण शीघ्र नहीं उठना चाहते, वरन् अधैर्य के कारण उठना चाहते हैं। इस अनावश्यक नकारात्मक गुण को धीरे-धीरे धैर्य के विकास द्वारा विजित कीजिए। तब आप एक साथ ३ या ४ घण्टे तक बैठ सकेंगे।
एक साधक जो समाधि प्राप्त करना चाहता है, उसका धैर्य टिट्टिभ पक्षी की भाँति होना चाहिए, जिसने अपनी चोंच से समुद्र को खाली करने का प्रयत्न किया। एक बार यदि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, तो भगवान् उसकी सहायता अवश्य करने के लिए आयेंगे, जिस प्रकार गरुण टिट्टिभ पक्षी के लिए आये थे। सत्कर्म में सभी प्राणियों के लिए सहायता अनिवार्यतः आती है। यहाँ तक कि सीता को बचाने में बन्दरों तथा गिलहरियों ने भी श्री राम की सहायता की। वह जो आत्म-संयम, साहस, वीरता, सहन-शक्ति, धैर्य, दृढ़ता, शक्ति तथा निपुणता से युक्त है, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपको कभी भी अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे आपको अलंघ्य परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े।
१६. स्वतन्त्र प्रकृति
कुछ लोग कुछ वर्षों तक स्वतन्त्र रूप से ध्यान करते हैं। बाद में उनको वास्तव में गुरु की आवश्यकता का अनुभव होता है। उनके मार्ग में कुछ रोड़े आते हैं। वे नहीं जानते कि आगे कैसे बढ़ें और इन बाधाओं को किस प्रकार पार किया जाये। तब वे गुरु की खोज प्रारम्भ करते हैं। एक परदेशी को दिन के समय में भी एक शहर में स्थित गली में अपने निवास वापस जाना कठिन अनुभव होता है, चाहे वह पैदल आधा दर्जन बार वहाँ गया हो। जब शहरों में ही रास्ता ढूँढ़ने में इतनी परेशानी होती है, तो आध्यात्मिक के तेज धार वाले रास्ते में परेशानी के बारे में कहना ही क्या, जहाँ व्यक्ति को आँखें बन्द करके अकेले चलना है।
मन को पुराने चक्रों, लीकों में जाने न दें। जब यह ध्यान में नीचे आये, तो उसे तुरन्त ही उठायें। नवीन दैवी स्पन्दन तथा विचार-तरंगें उत्पन्न करें। प्रार्थना करें। गीता के श्लोक दोहरायें।
निरर्थक विचार करने से ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। निरर्थक, अनिष्ट विचारों को भगा कर मानसिक ऊर्जा का सरंक्षण करें। तब आप ध्यान में विकास करेंगे।
जिस प्रकार जब पानी खेतों में सही नालियों में से जाने के स्थान पर चूहे के बिलों में बह जाता है, तो यह व्यर्थ चला जाता है और पौधों तथा फलदार वृक्षों एवं अनाज आदि के विकास में सहायता नहीं करता, उसी प्रकार यदि साधक के पास सच्चा वैराग्य नहीं होता, तो उसके ध्यान के प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं, उसकी ध्यान में प्रगति नहीं होती।
यदि मन निरन्तर विषय-वस्तुओं में लगा रहे, तो विश्व की यथार्थता की धारणा में निश्चय ही वृद्धि होगी। यदि मन निरन्तर आत्मा के बारे में विचार करता है, तो संसार स्वप्न जैसा प्रकट होता है।
१७. ईर्ष्या
यह भी एक महान् बाधा है। यहाँ तक कि वे साधु जिन्होंने सब चीजें छोड़ दी हैं, जो हिमालय में गंगोत्री और उत्तरकाशी की गुफाओं में मात्र एक कौपीन पहन कर रहते हैं, वे भी इस वृत्ति से मुक्त नहीं हैं। साधु गृहस्थों से अधिक ईर्ष्यालु होते हैं। जब कोई साधु ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में रहता है और जब वे देखते हैं कि पड़ोसी साधु का लोग आदर और सम्मान करते हैं, तो उनका हृदय जल जाता है। वे पड़ोसी को कलंकित करते हैं। और उसको नष्ट करने या बाहर निकालने की विधियाँ उपयोग करते हैं। कितना दयनीय दृश्य है! क्या ही शोचनीय दृश्य है! सोचने में भयानक! कल्पना करने में भी भयंकर! जब हृदय जलता है, तो आप मन की शान्ति की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? यहाँ तक कि बहुत अधिक पढ़े-लिखे लोग बहुत क्षुद्र मानसिकता वाले होते हैं। ईर्ष्या शान्ति और ज्ञान की सबसे बुरी शत्रु है। यह माया का सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार है। साधकों को सावधान रहना चाहिए। उनको नाम, यश और ईष्या का दास नहीं बनना चाहिए। यदि उसमें ईर्ष्या है, तो वह मात्र एक क्षुद्र प्राणी है। वह भगवान् से दूर है। व्यक्ति को अन्यों के कल्याण में आनन्दित होना चाहिए। व्यक्ति जब अन्यों को समृद्धिशाली स्थिति में देखे, तब उसे मुदिता का विकास करना चाहिए। उसे सभी प्राणियों में आत्म-भाव का अनुभव करना चाहिए। ईर्ष्या अनेक रूप ग्रहण कर लेती है जैसे ईर्ष्या, असूया, • मात्सर्य आदि। ईर्ष्या के सभी रूपों का पूर्णतया उन्मूलन कर देना चाहिए। जिस प्रकार दूध उबालने की प्रक्रिया में बार-बार उबलता है, उसी प्रकार ईर्ष्या बार-बार फूट पड़ती है। इसका पूर्णतया उन्मूलन कर देना चाहिए।
१८. निम्न प्रकृति
१. क्षुद्र हठी अहंकार जो मानवीय व्यक्तित्व को प्रेरक गति देता है, वह ध्यान अथवा आत्म-साक्षात्कार के मार्ग में गम्भीर बाधा है। यह क्षुद्र आत्म अहंकारी तत्त्व इसके सतही विचारों को सहारा देता है तथा इसकी भावनाओं, चरित्र तथा कार्य के आदतन मार्गों को दबाता है। यह राजसिक तथा तामसिक अहं है जो उच्च, दैवी सात्त्विक प्रकृति को आवृत करता है। यह स्वप्रकाश्य अमर आत्मा को आवृत करता है।
आपको सत्य की अभिलाषा होनी चाहिए। आपको भक्ति से पूर्ण होना चाहिए। आपमें बाधाओं तथा बलों पर विजय की इच्छा होनी चाहिए। यदि यह क्षुद्र अहं हठी रहेगा अथवा स्थायी रहेगा, यदि आप बाह्य व्यक्तित्व परिर्वतन अथवा रूपान्तरण हेतु सहमत नहीं हैं, तो आप आध्यात्मिक पथ में तेजी से प्रगति नहीं कर सकेंगे। इसके स्वयं के अपने तरीके और मनोवृत्तियाँ होंगी।
निम्न प्रकृति का पूर्णतया नवीनीकरण किया जाना चाहिए। साधक के आदतन निम्न व्यक्तित्व को पूर्णतया परिवर्तित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो किसी भी आध्यात्मिक अनुभव अथवा शक्ति का कोई मोल नहीं है। यदि यह क्षुद्र अहं अथवा मानव-व्यक्तित्व में यह क्षुद्र सीमित स्वार्थपूर्ण निम्न मानवीय चेतना बनी रहे, तो कितनी भी साधना या तपस्या का कोई परिणाम नहीं प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि आपको भगवद्-साक्षात्कार हेतु सच्ची अभिलाषा नहीं है। यह मात्र उत्सुकता से अधिक कुछ नहीं है। साधक गुरु से कहता है—“मैं योगाभ्यास करना चाहता हूँ, मैं निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ।” लेकिन वह अपनी निम्न प्रकृति को बदलना नहीं चाहता। वह अपने स्वयं के तरीके और पुरानी आदतें, पुराना चरित्र तथा व्यवहार बनाये रखना चाहता है।
यदि कोई साधक अथवा योगाभ्यासी अपनी निम्न प्रकृति को बदलना अस्वीकार कर देता है अथवा यदि वह अपने निम्न आदतन व्यक्तित्व में परिवर्तन को अस्वीकार कर देता है, तो वह किंचित् भी सच्चा आध्यात्मिक उत्थान नहीं कर सकेगा। निम्न प्रकृति अथवा स्वाभाविक तुच्छ व्यक्तित्व का पूर्ण रूपान्तरण किये बिना कोई भी आंशिक अथवा अस्थाई उत्थान, किसी भावोत्कर्ष के क्षणों में कभी-कभी होने वाली आकांक्षा, कभी-कभी भीतर से क्षणिक आध्यात्मिक भाव, इन सबका निम्न प्रकृति में। परिवर्तन के बिना कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है।
निम्न प्रकृति का परिवर्तन सरल नहीं है। आदत का बल सदैव शक्तिशाली और विपरीत है। इसके लिए महत् इच्छा-शक्ति चाहिए। साधक अक्सर पुरानी आदतों के बल के सामने असहाय अनुभव करता है। उसे नियमित जप, कीर्तन, ध्यान, अथक निष्काम सेवा, सत्संग के द्वारा सत्त्व संकल्प का विकास करना होगा। उसे अन्तरावलोकन करना चाहिए तथा अपने स्वयं के दोष तथा दुर्बलताओं को ढूँढ निकालना चाहिए। उसे अपने गुरु के निर्देशन में रहना चाहिए। गुरु उसके दोष ढूँढ निकालेंगे और उनके उन्मूलन के लिए अनुकूल तरीके खोज निकालेंगे।
२. यदि निम्न प्रकृति हठी और स्वाग्रही है तथा यदि यह क्षुद्र मन तथा इच्छा से समर्थित एवं न्यायसंगत ठहरायी जा रही हो, तब मामला बहुत गम्भीर बन जाता है। वह बिगड़ा हुआ, अशान्त, उद्दण्ड (बेलगाम), हठी तथा धृष्ट बन जाता है। वह सभी नियमों तथा अनुशासनों को तोड़ता है।
ऐसा साधक अपनी पुरानी आत्मा से चिपका रहता है। उसने न तो भगवान् को और न ही अपने गुरु को स्वयं को समर्पित किया है। वह छोटी-सी चीज के लिए किसी भी व्यक्ति से बदला लेने को तैयार रहता है। वह कभी आज्ञा का पालन नहीं करता। वह कोई भी आध्यात्मिक निर्देश नहीं ग्रहण करना चाहता। वह स्वेच्छाचारी, आत्मसन्तुष्ट तथा आत्मपूर्ण है। वह अपनी कमजोरियों तथा दोषों को स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता। वह सोचता है कि वह महान है। वह भाग्याधीन जीवन व्यतीत करता है।
पुराना व्यक्तित्व इसकी निम्न प्रकृति के पूर्व रूपों के साथ स्वयं ही दृढ़ होता है। वह दृढ़ होता है और अपनी सुविधा के अनुसार स्वयं के अपरिष्कृत एवं अहंकारी विचारों, कामनाओं, कल्पनाओं का अनुकरण करता है। वह अपनी न बदलने वाली, आसुरी तथा झूठी प्रवृत्ति को इसकी असत्यता, स्वार्थता तथा क्रूरता सहित अनुकरण करना तथा इसे अपनी बातों, कार्यों एवं व्यवहार में अभिव्यक्त करना अपना अधिकार समझता है।
वह उग्रतापूर्वक तर्क करता है तथा स्वयं का विभिन्न तरीकों से बचाव करता है। और विशेष प्रकार से इनको ढाँकता है। वह स्वयं के सोचने, बोलने तथा भाव क आदतन पूर्व-तरीकों को निरन्तर दोहराने का प्रयत्न करता है।
वह स्वीकार एक चीज को करता है और व्यवहार दूसरी चीज का करता है। वह अपने गलत दृष्टिकोणों को स्वीकार करने हेतु अन्यों पर बल डालता है। यदि अन्य लोग उसके गलत दृष्टिकोणों को स्वीकार करने हेतु इच्छुक नहीं होते, तो वह उनसे लड़ने को तैयार हो जाता है। वह तुरन्त विद्रोह करने हेतु खड़ा हो जाता है। वह मानता है कि मात्र उसका दृष्टिकोण सही है तथा जो उसके दृष्टिकोण का विरोध करते हैं, वे बेईमान, विचारशून्य तथा अशिक्षित हैं। वह अन्य लोगों को समझाना चाहता है कि उसका मार्ग एवं दृष्टिकोण योगविद्या के पूर्ण अनुरूप है। आश्चर्यजनक लोग हैं वे ! वास्तव में संसार को ऐसे अद्भुत लोगों की आवश्यकता नहीं है।
यदि वह स्वयं के प्रति सरल तथा अपने गुरु के प्रति निष्कपट है, यदि वह वास्तव में स्वयं को सुधारना चाहता है, तो वह अपनी अज्ञानता एवं दोषों को स्वीकार करने लगेगा तथा वह अपने प्रतिरोध के स्रोत एवं प्रकृति को पहचानने लगेगा। वह शीघ्र ही स्वयं को सुधारने तथा परिवर्तन करने हेतु सीधे रास्ते पर होगा। लेकिन वह किसी सफाई अथवा तर्क अथवा अन्य सहारे से अपने पुराने आसुरी स्वभाव या पुराने आसुरी विचार को गुप्त रखने का प्रयत्न करता है।
३. स्वाग्रही तथा अभिमानी साधक समाज में एक व्यक्तित्व बनने का प्रयास करते हैं। वे समाज में एक स्थिति तथा प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं। वे ऐसे बनते हैं जैसे वे एक महान् योगी हैं तथा उनके पास कई यौगिक सिद्धियाँ हैं। वे एक उच्च साधक अथवा उच्च योगी की भाँति, जिनको महान् ज्ञान तथा अनुभव अथवा निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गयी है, स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। यह अज्ञान, अभिमान तथा पूर्ण राजसिकता अधिकांश लोगों में थोड़ी मात्रा में तो विद्यमान होती ही है।
वह गुरु के आदेश का पालन करने तथा बड़े एवं श्रेष्ठ जनों का आदर करने की इच्छा नहीं रखता। वह अनुशासन तोड़ने को हमेशा तैयार रहता है। उसके स्वयं के विचार तथा भावनाएँ होती हैं। आदेश का पालन न करना तथा अनुशासन तोड़ना उसमें बीज रूप में होता है। वह कभी वादा करता है कि वह अपने गुरु तथा बड़ों का आज्ञापालक शिष्य रहेगा, लेकिन शीघ्र ही उसके कार्य उसके वचनों के विपरीत होते हैं। अनुशासन का पालन न करना ही वास्तव में साधक की महान् बाधा है। वह अन्यों के सामने सबसे बुरा उदाहरण प्रस्तुत करता है।
जो आज्ञा का पालन नहीं करता, जो नियम तोड़ता है, जो अपने गुरु से निष्कपट नहीं है, जो अपना हृदय अपने आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक के समक्ष नहीं खोल सकता, वह गुरु की सहायता से लाभान्वित नहीं हो सकता।
वह अपने स्वनिर्मित दलदल अथवा कीचड़ में फँसा रहता है तथा दैवी पथ में प्रगति नहीं कर सकता। कितनी दयनीय बात है! उसका भाग्य सच में ही शोचनीय है।
वह कपटाचरण करता है। वह ढोंग करता है। वह बातों को बढ़ा-चढ़ा कर रखता है। वह झूठा स्वाँग रचता है। वह अपनी कल्पना का झूठा उपयोग करता है। वह अपने विचारों तथा तथ्यों को गुप्त रखता है। वह तथ्यों को तोड़ता-मरोड़ता है और तथ्यों को गोपनीय रखने से इन्कार कर देता है। वह भयंकर झूठ बोलता है। वह ऐसा अपनी अनुशासनहीनता अथवा अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिए किये गये गलत कार्यों को ढाँकने के लिए तथा अपने तरीके अथवा पुरानी आदतों तथा कामनाओं में लिए रहने के लिए करता है।
चूँकि उसकी बुद्धि अशुद्धता से आवृत रहती है, इस कारण वह स्वयं ही नहीं जानता कि वह वास्तव में क्या कर रहा है। वह नहीं जानता कि वह जो कह रहा है, उसका क्या अर्थ है।
वह अपनी गलतियाँ और दोषों को स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक कि यदि कोई उसे सुधारने के लिए उसके दोष बताता है, तो उसे अत्यधिक क्रोध आ जाता है। वह उससे झगड़ा करने लगता है। उसके भीतर अत्यधिक पाशविकता है।
उसे आत्म-समर्थन की बहुत खतरनाक आदत है। वह सदा किसी भी प्रकार के मूर्खतापूर्ण तर्क, चालबाजी आदि के द्वारा अपनी स्थिति, अपनी बातों को सही बताने, अपने विचारों पर चिपके रहने, अपनी स्थिति और अपने कार्यों को बनाये रखने का प्रयत्न करता है। यह गुण कुछ में कम मात्रा में तथा कुछ में अधिक मात्रा में होते हैं।
४. यदि वह अपनी वर्तमान दुःखद स्थिति के लिए थोड़ा भी बुरा अनुभव करता है, यदि वह थोड़ा भी सुधार दिखाने का प्रयत्न करता है, यदि वहाँ थोड़ा भी ग्राह्य व्यवहार होता है, तो वह सुधर सकता है। वह योग के मार्ग में प्रगति कर सकता है। यदि वह स्वेच्छाचारी तथा हठी है, यदि वह पूर्णतः हठी है और यदि उसने अपनी आँखें बन्द कर रखी है अथवा सत्य के अथवा दैवी प्रकाश के विरुद्ध अपना हृदय कड़ा कर लिया है, तो कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता।
साधक को अपनी पूर्ण सम्मति अपने सर्वभाव के साथ अपनी निम्न प्रकृति को दैवी प्रकृति में बदलने हेतु सौंप देना चाहिए। उसे भगवान् अथवा गुरु के प्रति पूर्ण, निःशर्त प्रसन्तापूर्वक आत्म-समर्पण करना चाहिए। उसका सच्चा भाव तथा सही स्थायी व्यवहार होना चाहिए। उसे सही दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए। मात्र तभी सच्चा परिवर्तन आयेगा। मात्र सिर हिलाने, पसीना बहाने अथवा 'हाँ' कहने से कोई काम नहीं होगा। यह आपको महान् व्यक्ति अथवा योगी बनायेगा।
योग का मात्र वे ही अभ्यास कर सकते हैं, जो कि इसके प्रति बड़े लगनशील हैं तथा जो अपने क्षुद्र अहंकार तथा इसकी माँगों का उन्मूलन करने को तैयार हैं। आध्यात्मिक पथ में आधा माप कोई नहीं है। मन तथा इन्द्रियों का कठोर संयम, कठोर तपस्या तथा निरन्तर ध्यान भगवद्-साक्षात्कार हेतु अनिवार्य हैं। यदि आप जागरूक नहीं हैं, यदि आप थोड़ी-सी छूट अथवा छोटा-सा मार्ग उन्हें दे दें, तो विरोधी बल आपको भ्रमित करने हेतु तैयार हैं। यदि आप अपनी पुरानी क्षुद्र आत्मा, पुरानी आदतें, पुरानी हठी निम्न प्रकृति से चिपके रहे, तो योग का अभ्यास नहीं किया जा सकता।
आप एक साथ दो तरह का जीवन नहीं बिता सकते। शुद्ध दैवी जीवन, योगमय जीवन वासना तथा अज्ञान के नश्वर जीवन के साथ नहीं रह सकता। दैवी जीवन तुम्हारे स्वयं के क्षुद्र स्तर के अनुरूप नहीं हो सकता। आपको क्षुद्र मानवीय स्तर से ऊपर उठना ही होगा। आपको स्वयं को दैवी चेतना के उच्च स्तर तक उठाना होगा। यदि आप एक योगी बनना चाहते हैं, तो आप अपने क्षुद्र मन तथा क्षुद्र अहंकार के प्रति स्वतन्त्रता का दावा नहीं कर सकते हैं।
आपको स्वयं अपने विचारों, निर्णय, कामनाओं तथा आवेगों को दृढ़ नहीं करना चाहिए। निम्न प्रकृति अपने परिजनों—हठ, अज्ञानता तथा अशान्ति के सहित दैवी प्रकाश के मार्ग में खड़ी है।
योग-मार्ग में एक सच्चे गम्भीर साधक बनिए। इस निम्न प्रकृति को उच्च दैवी प्रकृति का विकास करने के द्वारा नष्ट कर दीजिए। ऊँचे उड़िए। दैवी प्रकाश के स्वागत के लिए स्वयं को तैयार रखिए। स्वयं को शुद्ध कीजिए तथा एक कर्मशील योगी बनिए।
महानू योगियों का आशीर्वाद आप सब पर हो!
१९. मनोराज्य
मनोराज्य का अर्थ है हवाई किले बनाना। यह मन की एक चाल है। इस आश्चर्य को देखिए। साधक हिमालय की एकान्त गुफा में ध्यान कर रहा है। वह गुफा में योजना बना रहा है-"अपना ध्यान समाप्त करने के बाद मैं सैन फ्रांसिस्को, न्यूयार्क में जाऊँगा तथा वहाँ प्रवचन दूंगा। मैं कोलम्बिया में एक आध्यात्मिक गतिविधि का केन्द्र बनाऊँगा। मुझे संसार में कुछ नया करना है। मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया गया हो।” यह महत्त्वाकांक्षा है। यह अहंकारिक कल्पना है। यह महान् बाधा है। यह शक्तिशाली विघ्न है। यह मन को एक सेकेंड के लिए भी विश्राम नहीं करने देती। बार-बार वहाँ कोई-न-कोई योजना का पुनः जन्म होता रहता है। साधक सोचेगा कि उसका बड़ा गहन ध्यान लग गया है, लेकिन यदि वह अन्तरावलोकन तथा आत्म-विश्लेषण द्वारा मन को निकट से देखे, तो यह शुद्ध मनोराज्य का मामला होगा। एक मनोराज्य विलीन होगा, तो दूसरा पलक झपकते ही निर्मित हो जायेगा। यह मन रूपी झील में छोटी-सी लहर अथवा छोटा संकल्प होगा। लेकिन बार-बार विचार करने से यह कुछ ही मिनट में अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेगा। कल्पना की शक्ति अद्भुत है। माया कल्पना-शक्ति के द्वारा बड़ा विनाश करती है। कल्पना मन को स्थूल कर देती है। कल्पना कस्तूरी मृग या सिद्धमकरध्वज है। यह मरते हुए मन को पुनर्जीवित करती है। कल्पना शक्ति मन को एक पल के लिए भी शान्त नहीं रहने देती। जिस प्रकार शलभ अथवा मधुमक्खियों का झुण्ड एक सतत प्रवाह की तरह आता है, उसी प्रकार मनोराज्य की तरंगें निरन्तर प्रवाह से आती रहती हैं। विचार, विवेक, प्रार्थना, जप, ध्यान, सत्संग, उपवास, प्राणायाम तथा निर्विचारता का अभ्यास इस बाधा को दूर कर कर देगा। प्राणायाम मन की गति को रोकेगा तथा मन को शान्त करेगा। एक तरुण आकांक्षी मनुष्य एक एकान्त गुफा में रहने हेतु अयोग्य है। जिसने संसार में रह कर कुछ वर्षों तक निष्काम सेवा की हो तथा जिसने समतलों में एकान्त कमरे में रह कर कुछ वर्षों तक ध्यान का अभ्यास किया हो, वह गुफा में निवास कर सकता है। मात्र ऐसा ही मनुष्य हिमालय के जंगलों के एकान्त में सच्चा आनन्द उठा सकता है।
जब आप महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि' अथवा 'तत्त्वमसि' के अर्थ पर महावाक्यानुसन्धान की विधि से निरन्तर ध्यान करते हैं, तो सभी विषय (देखना, सुनना, स्पर्श, स्वाद तथा सूँघना) रुक जायेंगे। लेकिन संस्कारों के बल के कारण मनोराज्य चलता रहेगा। निद्रा भी प्रवेश करेगी। लेकिन यदि आप जागरूक हैं, तो सतत प्रयत्न और निरन्तर स्वरूप-चिन्तन (ब्रह्म पर ध्यान) द्वारा आप इन दोनों बाधाओं से मुक्ति पा सकेंगे। तब स्थिर ब्रह्माकार-वृत्ति तथा ब्रह्मज्ञान शीघ्र आयेगा। अज्ञान नही हो जायेगा। आप सहज परमानन्द अवस्था में स्थापित हो जायेंगे। सभी संचित कर्म ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जायेंगे।
२०. स्मृति
जब आप ध्यान हेतु बैठेंगे, तो आपके मित्र और कार्यालय के काम के विचार और सन्ध्या के समय आपके मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ जो वार्तालाप हुआ, उसकी स्मृति आपके मन को बार-बार विचलित करेगी और बाधा डालेगी। आपको सजग रूप से मन को बार-बार बाह्य सांसारिक विचारों से वापस खींचना होगा तथा इसे अपने लक्ष्य अथवा बिन्दु पर केन्द्रित करना होगा। आपको सांसारिक विचारों की उपेक्षा करनी होगी। निरपेक्ष रहें। इन विचारों का स्वागत न करें। स्वयं को इन विचारों के साथ न जोड़ें। स्वयं से कहें — “मैं ये विचार नहीं चाहता। मैं इन विचारों के साथ कुछ नहीं करने वाला। वे धीरे-धीरे नष्ट हो जायेंगे।"
चाहे आप हिमालय की किसी एकान्त गुफा में निवास करें, चाहे आप ध्यान का अभ्यास करें, यदि पुराने अनुभवों की स्मृति आयेगी और यदि आप मन को इसमें बार-बार लीन होने देंगे, तो चाहे आपका निवास हिमालय के एकान्त वन में हो, लेकिन फिर भी आप गुफा में पूर्ण दिव्य जीवन नहीं बिता रहे हैं, क्योंकि आप पवित्र गुहा में भी पुराना सांसारिक जीवन बार-बार व्यक्तिगत रूप से बिता रहे हैं। विचार ही वास्तविक कर्म हैं।
जब आप योग की सीढ़ी पर चढ़ें, जब आप आध्यात्मिक पथ पर चलें, तो पीछे न देखें। अपने भूतकाल के अनुभवों का स्मरण न करें। भूतकाल के सभी अनुभवों को मार दें। दृढ़तापूर्वक अपना मानसिक भाव निर्मित करें—“मैं ब्रह्म हूँ।”
इस पर टिके रहें। बार-बार ब्रह्माकार-वृत्ति उत्पन्न करें। नियमित एवं निरन्तर ध्यान द्वारा इसे स्थिर बनाये रखें। भूतकाल के अनुभव का एक अकेला विचार विचार-प्रतिबिम्ब या स्मृति-चित्र को नया जीवन देगा। इसे पुनर्जीवित अथवा दृढ़ करना आपको नीचे गिरा देगा। आपके लिए पुनः ऊपर चढ़ना कठिन होगा।
यदि भूतकाल के अनुभव की स्मृति बार-बार आयेगी, तो पुराने मानसिक चित्र ऊर्जा प्राप्त करेंगे अथवा शक्तिशाली हो जायेंगे। वे स्वयं को दुगनी शक्ति के साथ बार-बार अभिव्यक्त करेंगे। वे एक साथ एकत्रित होंगे या बहुगुणित हो कर अथवा एक समूह में आ कर आप पर भयंकर रूप से आक्रमण करेंगे। इसलिए पीछे न देखें। भूतकाल के अनुभवों की स्मृति को भगवान् के स्मरण द्वारा नष्ट करें।
स्वयं को मात्र वर्तमान से सम्बद्ध रखे। भूतकाल अथवा भविष्य की ओर पीछे की ओर मुड़ कर न देखें। ऐसा करने पर ही आप प्रसन्न रह सकते हैं। तब आप देखभाल, चिन्ताओं तथा आकुलताओं से मुक्त होगे। आप दीर्घायु होंगे। कठोर प्रयत्नों के द्वारा संकल्पों को नष्ट कर दें। सच्चिदानन्द ब्रह्म पर निरन्तर ध्यान करें तथा उस परमात्मा के निर्मल पद को प्राप्त करें। आप सफलता प्राप्त करें। आप ब्रह्मानन्द में एक ज्ञानावस्था में ब्रह्मानन्द के सागर में स्नान करते हुए ज्ञान अवस्था में निवास करें।
विचार और विवेक का अपने प्रयत्नों में प्रयोग करें। भूत तथा भविष्य के बारे में विचार न करें। जब आप चालीस वर्ष के हो जायेंगे, तो भूतकाल के तरुणाई के दिन और स्कूल के दिन सभी स्वप्न मात्र होंगे। सम्पूर्ण जीवन एक दीर्घ स्वप्न है। अब भूतकाल आपके लिए एक स्वप्न है। भविष्य भी अब ऐसा ही है। आपको मात्र वर्तमान से व्यवहार करना है। आपको मन रूपी चिड़िया के दोनों पंख काट देने हैं। दोनों पंख भूत और भविष्य को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन यह फड़फड़ाता है, क्योंकि वहाँ वर्तमान है। सभी बाह्य संस्कारों को दूर कर दें। वृत्तियों को बन्द करें। मन को शान्त करें। मन के रूपान्तरणों को रोकें। धारणा करें। संस्कारों के परिणाम जो कि विचार हैं, उनके बहुगुणित होने पर विजय पायें। मन को ध्यान हेतु एक अच्छा भोजन-गीता के कुछ श्रेष्ठ विचार, अवधूतगीता, ॐ का अर्थ आदि दें। कुछ समय बाद गुप्त वर्तमान भी नष्ट हो जायेगा। मन पूर्णतया शान्त एवं स्थिर बन जायेगा। आत्मा का सर्वोच्च ज्ञान आपके शुद्ध मन में आयेगा। आप ब्रह्म अधिष्ठान में स्रोत, अवलम्बन, प्रत्येक वस्तु के आधार और पृष्ठभूमि में विश्राम करेंगे। आप ज्ञाननिष्ठा अर्थात् स्वरूपस्थिति (सत्-चित्-आनन्द अवस्था) प्राप्त करेंगे।
२१. मानसिक वार्तालाप
ध्यान के समय आप मानसिक रूप से किसी से जल्दी-जल्दी बातें करेंगे। इस बुरी आदत को रोक दें। मन के ऊपर सावधानीपूर्वक ध्यान रखें।
२२. मोह
अब एक अन्य बाधा आती है, जिसने श्री शंकर को भी परेशान किया। उन्हें अपनी माँ की बीमारी तथा दाह-संस्कार में जाना पड़ा, जब कि वे एक संन्यासी थे। दक्षिण भारत के एक महान् सन्त पट्टिनानु स्वामी जी ने अपनी माँ की मृत्यु के समय गाया- "सबसे पहले त्रिपुर-संहार में अग्नि जली थी। उसके बाद लंका में अग्नि हनुमान् ने जलायी। अब मेरी प्रिय माँ की मृत्यु पर मेरे पेट और हृदय में अग्नि जल गयी है। अब मुझे अपनी माँ के शव को भी अग्नि लगानी होगी।” व्यक्ति के स्वयं के शरीर, पत्नी, पिता, माँ, भाई, बहन तथा धन के प्रति आसक्तिपूर्ण प्रेम को मोह कहते हैं। लोभ की भाँति मोह विभिन्न सूक्ष्म रूप ले लेता है। मन एक या अन्य नाम तथा रूप से चिपक जाता है।
बन्दरों के मोह को देखिए। अगर बन्दर का बच्चा मर जाता है, तो माँ उसके कंकाल को दो-तीन महीनों तक अपने शरीर से चिपकाये हुए घूमती रहती है। ऐसी मोह की शक्ति है। माया रहस्यमय है। यदि पिता को एक टेलीग्राम मिलता है कि उसके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गयी है, तो उसे तुरन्त झटका लगता है और वह बेहोश हो जाता है, कभी-कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यह मोह की शक्ति है। यह सारा संसार मोह से चल रहा है। यह मोह है जिसके द्वारा व्यक्ति संसार से बँधा है।
व्यक्ति मोह के द्वारा दुःख पाता है। मोह से आसक्ति होती है। मोह एक शक्तिशाली शराब है जो पलक झपकते ही नाश लाती है। यहाँ तक कि संन्यासियों को भी उनके आश्रम तथा शिष्यों के प्रति मोह हो जाता है। विवेक, वैराग्य, विचार, आत्म-चिन्तन, भक्ति, एकान्त तथा वेदान्तिक साहित्य का अध्ययन आदि के द्वारा मोह का उन्मूलन किया जा सकता है। मात्र संन्यास तथा आत्म-साक्षात्कार के द्वारा मोह को दग्ध किया जा सकता है।
जब पिछले युद्ध में करोड़ों लोग मर गये, तो आप तो कभी नहीं रोये; लेकिन जब आपकी पत्नी की मृत्यु हुई, तो आप फूट-फूट कर रोये। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उसके प्रति मोह था। मोह मेरे पन का विचार निर्मित करता है, इसलिए आप कहते हैं- “मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा घोड़ा।" यह बन्धन है, यह मृत्यु है। मोह विषय-वस्तुओं के प्रति आसक्ति उत्पन्न करता है। मोह भ्रम उत्पन्न करता है और बुद्धि को आवृत कर लेता है। मोह के बल द्वारा आप अवास्तविक गन्दे शरीर को वास्तविक शुद्ध आत्मा समझ लेते हैं। आप अवास्तविक संसार को ठोस सच्चाई समझ लेते हैं। ये मोह के कार्य हैं। मोह माया का शक्तिशाली अस्त्र है।
२३. योग में बाधाएँ
(पतंजलि के राजयोग से)
रोग, सुस्ती, सन्देह, लापरवाही, आलस्य, अज्ञानता, सांसारिक बुद्धि, वैषयिकता, भ्रम, लक्ष्य का चूकना, अस्थिरता, मन का विचलन —ये सभी बाधाएँ हैं। रोग वायु, पित्त तथा कफ के सन्तुलन बिगड़ जाने से उत्पन्न होते हैं। यदि कफ अधिक होगा, तो आपका शरीर भारी हो जायेगा, जिसके कारण आप आसन में अधिक देर तक नहीं बैठ सकेंगे। यदि मन में अधिक तमोगुण होगा, तो आप आलसी बन जायेंगे। रोग भोजन लेने में अनियमितता, कुपोषणयुक्त भोजन लेने (जो कि शरीर के लिए अनुकूल न हो), रात को देर तक जागने, वीर्य के नाश तथा मल-मूत्र के रोकने से होते हैं। आसन, प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम, ध्यान का अभ्यास, आहार में समन्वय, उपवास, रेचक, एनिमा, स्नान, सूर्य-उपचार, पर्याप्त विश्राम आदि से रोग दूर किये जा सकते हैं। सर्वप्रथम विषय को पहचानें तथा रोग का कारण ढूँढ़ें, तत्पश्चात् उपचार का प्रयत्न करें अथवा किसी डाक्टर से सलाह लें।
सुस्ती में पथ में अनुभवहीनता के कारण अथवा पूर्व-जन्मों के संस्कारों की कमी के कारण व्यक्ति किसी भी साधना हेतु अयोग्य होता है। मन की कार्य करने हेतु इच्छा न होना, उदासी, आलस्य आदि को सुस्ती कहते हैं। इसे प्राणायाम, आसन तथा कार्य करते रहने की आदत से दूर किया जा सकता है। यह है या वह है, ऐसा सोचना सन्देह है। साधक सन्देह करता है कि योग शास्त्र सत्य हैं अथवा नहीं। इसको सही ज्ञान, विवेक, विचार, शास्त्रों के अध्ययन तथा महात्माओं के साथ सत्संग के द्वारा दूर किया जा सकता है।
अविरति मन की प्रवृत्ति है जो कि अविरत रूप से मोह के कारण किसी-न-किसी विषय के आनन्द के प्रति तीव्र अभिलाषा करता है। यह वैराग्य, सांसारिक विषयों तथा सांसारिक जीवन के दोषों जैसे अस्थायित्व, रोग, मृत्यु, जरावस्था, कष्टों आदि में दृष्टि रखने तथा वैरागी महात्माओं के साथ निरन्तर सत्संग करने तथा वैराग्य से सम्बन्धित पुस्तकों के अध्ययन से दूर किया जा सकता है।
भ्रान्ति-दर्शन जैसी अनावश्यक स्थिति को भी गलती से अत्यधिक आवश्यक मान लिया जाता है। सच्चे मार्ग से भटकना, समाधि तथा सिद्धियों के चक्कर में पड़ना इनको लक्ष्य को चूकना कहते हैं। लक्ष्य को चूकना तथा अस्थायित्व को और अधिक वैराग्य के विकास तथा एकान्त में निरन्तर प्रबल साधना करने के द्वारा दूर किया जा सकता है। अस्थायित्व या अस्थिरता मन की अस्थिरता है, यह योगी को समाधि अवस्था में नहीं रहने देती है, चाहे वह यहाँ तक कितनी अधिक कठिनाई के बाद पहुँचा हो। माया शक्तिशाली है। कप और होंठों के बीच कई फिसलनें हैं। जो ॐ का जप अध्याय २ के २८ वे सूत्र में बताये अनुसार करते हैं, उनके सामने ये बाधाएँ नहीं आती हैं।
जब थोड़ी परेशानी आये, तो अभ्यास को न रोकें। बाधाओं के उन्मूलन हेतु अनुकूल साधना खोजें। जब तक आप असम्प्रज्ञात समाधि तक न पहुँच जायें, आगे बढ़ते जायें। यदि आप लगनशील हैं और साधना में स्थिर हैं, तो सफलता आने को बाध्य होगी।
२४. अन्य बाधाएँ
यदि आप बेकार की गपशप तथा अन्यों के बारे में अफवाहें एवं समाचार सुनने की बेकार की उत्सुकता छोड़ सकते हैं तथा यदि आप अन्यों के मामलों के बीच में दखल नहीं दें, तो आपके पास ध्यान हेतु बहुत-सा समय होगा। ध्यान के समय मन को शान्त बनायें। यदि ध्यान के समय सांसारिक विचार मन में प्रवेश करना चाहें, तो उनकी उपेक्षा करें। सत्य के प्रति स्थिर समर्पण रखें। उत्साहपूर्ण रहें। अपने भीतर सत्त्व में वृद्धि करें। आप स्थायी आनन्द का उपभोग करेंगे।
वातावरण बुरा नहीं है, बल्कि आपका मन बुरा है। आपका मन उचित प्रकार से अनुशासित नहीं है। इस भयंकर मन के साथ युद्ध करें। बुरे वातावरण के विरुद्ध शिकायत न करें, बल्कि सबसे पहले स्वयं अपने मन के प्रति शिकायत करें। सबसे पहले मन को प्रशिक्षित करें। यदि आप विपरीत वातावरण में ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो आप दृढ़तापूर्वक विकास करेंगे। आप शीघ्र संकल्प-शक्ति का विकास करेंगे तथा आप एक योगी बन जायेंगे। प्रत्येक चीज में अच्छाई देखें, बुराई को अच्छाई में बदल दें। यही सच्चा कार्य है।
ऊर्जा का बहना, वासनाओं की भीतरी तरंगें, इन्द्रियों के नियन्त्रण में कमी, साधना में गिरावट, वैराग्य में कमी, प्रबल अभीप्सा की कमी, साधना में अनियमितता —ये सभी धारणा के मार्ग की अनेक बाधाएँ हैं।
२५. पूर्वाग्रह, असहिष्णुता और हठधर्मिता
पूर्वाग्रह किसी भी चीज अथवा किसी व्यक्ति के प्रति अकारण ही नापसन्दगी है। यह मस्तिष्क को निर्मोही बना देती है। मस्तिष्क चीजों को उनके सही प्रकाश में ग्रहण करने हेतु उचित प्रकार से स्पन्दित नहीं हो पाता। व्यक्ति विचारों में सच्ची भिन्नता को सहन नहीं कर पाता। यह असहिष्णुता है। धार्मिक असहिष्णुता एवं पूर्वाग्रह भगवद्-साक्षात्कार में महानू बाधा हैं। कुछ रूढ़िवादी संस्कृत पण्डित सोचते हैं कि मात्र संस्कृत जानने वाले ही भगवद्-साक्षात्कार कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि अँग्रेजी जानने वाले संन्यासी भगवद्-साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते। यदि किसी का बाइबिल तथा कुरान के प्रति पूर्वाग्रह होगा, तो वह उन पुस्तकों के सत्यों को नहीं ग्रहण कर सकेगा। उसका मस्तिष्क कठोर होगा। कोई भी व्यक्ति कुरान, बाइबिल अथवा जैद-अवस्ता अथवा भगवान् बुद्ध की पुस्तकों में बताये गये सिद्धान्तों के अध्ययन एवं अनुकरण द्वारा भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है।
साधकों को सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करना चाहिए, तभी मात्र वे सर्वत्र सत्य के दर्शन कर सकेंगे। सत्य मात्र वाराणसी के संस्कृत पण्डितों अथवा अयोध्या के वैरागियों का एकाधिकार नहीं है। राम, कृष्ण, ईसामसीह सभी की साझा सम्पत्ति हैं।
रूढ़िवादी तथा हठधर्मी जन स्वयं को एक छोटे-से घेरे अथवा क्षेत्र में बन्द करके रखते हैं। उनका हृदय बड़ा नहीं होता। वे अपने दृष्टि-दोष के कारण अन्यों में अच्छी बात नहीं देख सकते। वे सोचते हैं कि मात्र उनके सिद्धान्त ही अच्छे हैं। वे अन्यों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। वे सोचते हैं कि मात्र उनका सम्प्रद्राय ही श्रेष्ठ है. तथा उनके गुरु ही एकमात्र भगवद्-साक्षात्कार प्राप्त हैं। वे हमेशा अन्यों के साथ झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन व्यक्ति को अन्य पैगम्बरों और सन्तों की शिक्षाओं का भी सम्मान करना चाहिए। मात्र तभी विश्व-प्रेम, वैश्विक भाईचारा प्रकट होगा। यह सभी प्राणियों में भगवद्-साक्षात्कार की ओर प्रेरित करेगा। पूर्वाग्रह, असहिष्णुता, हठधर्मिता, रूढ़िवादिता का पूर्णतया उन्मूलन किया जाना चाहिए। ये घृणा के रूप हैं।
२६. रजोगुण और तमोगुण
रजोगुण और तमोगुण ध्यान में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। जो मन ध्यान के समय सत्त्व की प्रबलता से शान्त रहता है, वह रजोगुण की अधिकता में प्रवेश करने से काँपने लगता है। संकल्पों (कल्पनाओं) की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बेचैनी बढ़ जाती है। कार्य के विचार प्रकट होते हैं। अन्तर में योजना बनाने का भाव प्रवेश करता है। थोड़ा विश्राम करें। पुनः जप करें। प्रार्थना करें तथा ध्यान करें। थोड़ा दूध ले लें।
२७. संकल्प
मन के मूल विचारों, विभिन्न निरर्थक संकल्पों (कल्पनाओं) से स्वयं को मुक्त करें। आत्मा का निरन्तर ध्यान करें। 'निरन्तर शब्द पर विशेष ध्यान दें। यह महत्त्वपूर्ण है। ऐसा करने पर ही मात्र आध्यात्मिक ज्ञान का आगमन होगा और ज्ञान-सूर्य चिदाकाश में उदित होगा।
२८. तमस्
अत्यन्त कम लोग ही सम्पूर्ण समय ध्यान हेतु उपयुक्त हैं। सदाशिव ब्रह्म तथा श्री शंकर के समान लोग ही मात्र सम्पूर्ण समय ध्यान हेतु लगा सकते हैं। अनेक साधु जो निवृत्ति-मार्ग ले लेते हैं, वे पूर्ण तामसिक बन जाते हैं। तमस् को सत्त्व मान लिया जाता है। यह महान् भूल है। कोई भी यदि यह जानता है कि अपना समय लाभदायक ढंग से किस प्रकार प्रयोग किया जाये, तो वह संसार में कर्मयोग करते हुए सुन्दर ढंग से विकास कर सकता है। एक गृहस्थ को समय-समय पर संन्यासियों एवं महात्माओं की सलाह लेते रहनी चाहिए। एक नियमित दिनचर्या बना लें और सांसारिक गतिविधियों के मध्य इस पर दृढ़ता से चिपके रहें। रजोगुण सतोगुण में परिवर्तित हो जायेगा। प्रबल रजस् एक सात्त्विक मोड़ लेता है। तमोगुण को अचानक सत्त्व में बदलना कठिन होता है। तमोगुण को सर्वप्रथम रजोगुण में बदलना चाहिए। जो युवा साधु निवृत्ति-मार्ग अपनाते हैं, वे अपनी दिनचर्या से चिपके नहीं रहते। वे बड़ों की बातें नहीं सुनते। वे गुरु के आदेश का पालन नहीं करते। वे प्रारम्भ से स्वतन्त्रता चाहते हैं। वे भाग्याधीन जीवन चाहते हैं। वहाँ उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनके अपने तरीके हैं। वे नहीं जानते कि ऊर्जा को किस प्रकार नियमित करें तथा किस प्रकार दैनिक दिनचर्या बनायें।
वे जगह-जगह निरुद्देश्य रूप से भटकते रहते हैं। वे छह माह में तामसिक बन जाते हैं। वे आधा घण्टे एक आसन में बैठते हैं और सोचते हैं कि वे साक्षात्कार प्राप्त आत्मा हैं। यदि एक साधक जिसने निवृत्ति-मार्ग ग्रहण कर लिया है, वह देखता है कि वह विकास नहीं कर रहा है और ध्यान में विकास नहीं कर रहा है, तो उसे तत्काल कुछ वर्षों तक सेवा करनी चाहिए तथा खूब काम करना चाहिए। उसे ध्यान के साथ काम को संयुक्त करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। यही समझदारी है। यह चतुराई है। उसके बाद उसे एकान्त में चले जाना चाहिए। व्यक्ति को सम्पूर्ण साधना में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। तामसिक अवस्था से बाहर आना बड़ा कठिन है। साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। जब तमोगुण उस पर विजय पाने का प्रयास करे, तो उसे तत्काल किसी प्रकार का कार्य तेजी से करना चाहिए। वह खुली हवा में दौड़ सकता है, कुँएँ से जल खींच सकता है। उसे कुछ बुद्धिमानीपूर्ण साधनों अथवा अन्य द्वारा तमोगुण को भगा देना चाहिए।
२९. तीन बाधाएँ
जब युवा साधक पूर्ण एकान्त तथा मौन धारण कर लें, तो उन्हें तीन बाधाओं का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए: १. निराशा, २. मनोराज्य तथा रसास्वाद तथा ३. गृहस्थों, पुरुषों और स्त्रियों के प्रति घृणा। वे मानवद्वेषी बन गये हैं। उन्हें उत्साहजनक विचारों का स्वागत करना चाहिए। मन को अक्सर देखें और सभी के प्रति शुद्ध प्रेम का विकिरण करें। यदि आपको ब्रह्मचर्य के पालन हेतु एक विधि अनुकूल न आये, तो आपको विभिन्न साधनाओं जैसे प्रार्थना, ध्यान, प्राणायाम, सत्संग, सात्त्विक आहार, एकान्त, विचार, शीर्षासन, सर्वांगासन, उड्डियान बन्ध, नौलि, अश्विनी मुद्रा, योग मुद्रा आदि को संयुक्त रूप से करना चाहिए। तभी आप सफल होंगे।
३०. तृष्णा और वासना
कामना अथवा तृष्णा शान्ति की शत्रु हैं। जो विषय-वस्तुओं के लिए तृषित हैं, उनके लिए किंचित् भी सुख नहीं है। जब यह तृष्णा मृत हो जाती है, तो मनुष्य शान्ति का आनन्द लेता है और मात्र तभी वह ध्यान कर सकता है और आत्मा में स्थित हो सकता है।
वासनाएँ बड़ी शक्तिशाली हैं। इन्द्रियाँ तथा मन बहुत उपद्रवी तथा प्रबल हैं। बार-बार युद्ध लड़ा जाना और विजित किया जाना चाहिए। यही कारण है आध्यात्मिक पथ को कठोपनिषद् में तलवार की धार पर चलना कहा गया है। दृढ़ संकल्पवान्, लौह संकल्पवान् पुरुष के लिए इस पथ में भी कोई कठिनाई नहीं है। प्रत्येक कदम पर भीतर से शक्ति प्राप्त होती है।
यदि आप भगवद्-साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो निरन्तर प्रयास अथवा निरन्तर उद्यम आवश्यक है । वासनाएँ, कामनाएँ, तृष्णाएँ तथा पुराने सांसारिक संस्कार पथ में बाधाएँ हैं। आन्तरिक संघर्ष बार-बार चलते रहना चाहिए।
३१. विक्षेप
विक्षेप मन का भटकाव है। यह मन की पुरानी आदत है। यह मन का विचलन है। सभी साधक सामान्यतया इस परेशानी के बारे में शिकायत करते हैं। इसमें मन एक बिन्दु पर लम्बे समय तक कभी नहीं टिकता। यह एक बन्दर के समान इधर-उधर कूदता रहता है। यह सदा बेचैन रहता है। यह रजोगुण के कारण होता है। जब भी श्री जयदयाल गोयनका मुझसे मिलने के लिए आये, तो उन्होंने मुझसे दो प्रश्न किये – “स्वामी जी, निद्रा पर नियन्त्रण का क्या उपाय है? विक्षेप को कैसे दूर किया जाये ? मुझे सरल और प्रभावकारी उपाय बताइए।" मेरा उत्तर था - " रात्रि में हलका भोजन लें। शीर्षासन और प्राणायाम करें।” इनसे निद्रा पर विजय प्राप्त होगी। त्राटक, उपासना, प्राणायाम तथा योग विक्षेप को दूर करेगा। अधिक अच्छा होगा यदि इन सबका संयुक्त रूप से अभ्यास किया जाये। यह अधिक प्रभावशाली होगा।
पतंजलि महर्षि के अनुसार रोग, मानसिक अकर्मण्यता, सन्देह, निरपेक्षता, आलस्य, विषय-सुख के पीछे भागना, संज्ञाहीन अवस्था, झूठा पूर्वानुमान, धारणा की प्राप्ति न होना तथा धारणा प्राप्त कर लेने पर बेचैनी के कारण उससे गिर जाना — ये सभी मुख्य विचलन हैं। उन्होंने रजोगुण जो कि विक्षेप को प्रेरित करते हैं, को नष्ट करने तथा एकाग्र मन प्राप्त करने के लिए प्राणायाम बताये हैं।
यदि आप मन का विचलन दूर कर सकें, तो आपको मन की एकाग्रता प्राप्त होगी। एकाग्रता ऐसी चीज है जो अनेकों को ज्ञात नहीं है। मैक्समुलर लिखता है - "एकाग्रता हमारे लिए (पश्चिमी लोगों के लिए) असम्भव है; क्योंकि हमारा मन समाचारपत्र, टेलीफोन, पत्राचार आदि के द्वारा विभिन्न दिशाओं में जाता रहता है।" सभी धार्मिक एवं दार्शनिक कल्पना एवं निदिध्यासन में एकाग्रता एक अनिवार्य स्थिति है।
गीता में भगवान् कृष्ण ने विक्षेप दूर करने के लिए एक साधना बतलायी है — “जब-जब मन भटके और अस्थिर हो, तो इसे अन्दर रोक कर आत्मा के नियन्त्रण में लाओ। कल्पना से जन्मी सभी कामनाओं को छोड़ कर मन के द्वारा इन्द्रियों को सब ओर से नियन्त्रित करके मन को आत्मा में रख कर इसे अन्य किसी के बारे में विचार न करने दो।” (अध्याय ६, श्लोक २४, २५ और २६)
त्राटक विक्षेप-नाश के लिए प्रभावशाली विधि है। इसका अभ्यास भगवान् कृष्ण के चित्र अथवा दीवार पर एक काले बिन्दु पर आधा घण्टे तक करें। सर्वप्रथम इसे दो मिनट तक करें और फिर धीरे-धीरे समय में वृद्धि करें। जब आँसू आने लगें, तब आँखें बन्द कर लें। आँखों पर जोर न डालें। आराम से देखें। 'कुण्डलिनीयोग' पुस्तक में इस क्रिया का पूर्ण विवरण पढ़ें।
एक दुर्बल साधक चाहे धारणा में दृढ़ हो, उस पर आलस्य विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक साधक यदि धारणा में दुर्बल है, तो वह विक्षेप द्वारा पराजित हो जाता है। इसलिए धारणा और ऊर्जा को सन्तुलित रखना चाहिए।
३२. विषयासक्ति
विषय-सुखों अथवा विषय-वस्तुओं के प्रति मोह को विषयासक्ति कहते हैं। यह सभी बाधाओं में सबसे बड़ी है। विषय-सुखों को पूर्णतया त्यागने से मन इन्कार कर देता है। वैराग्य तथा ध्यान के बल से कामनाएँ कुछ समय के लिए दब जाती हैं। अचानक मन आदत और स्मृति के कारण विषय-सुख के बारे में सोचता है। तब वहाँ मानसिक विघ्न उत्पन्न होता है। धारणा कम हो जाती है। मन विषय-वस्तुओं में बाहर घूमता है। गीता में आप पायेंगे — “हे कौन्तेय, यहाँ तक कि ज्ञानी पुरुष की उत्तेजित इन्द्रियाँ, चाहे वह प्रयत्न ही क्यों न कर रहा हो, उसके मन को उसी प्रकार बलात् खींच ले जाती हैं, जिस प्रकार लहरें जल पर से जहाज को खींच ले जाती हैं।” (अध्याय २, श्लोक ६० और ६७) “इन्द्रियों के विषय उसको (संयमी को) आनन्द नहीं देते, वे संयमी के शरीर से वापस लौट जाते हैं और यहाँ तक कि आनन्द भी परमात्मा के दर्शन के बाद उसके पास से वापस लौट जाता है।” (अध्याय २, श्लोक ५९)
कुछ कामनाएँ मन के कोने में छुपी रहती हैं। जब आप झाडू लगाते हैं, तो कमरे के कोने में छुपी धूल बाहर आती है, उसी प्रकार योगाभ्यास के दबाव से पुरानी छुपी हुई कामनाएँ दुगनी शक्ति से मन की सतह पर आती हैं। साधकों को बड़ा ही सावधान रहना चाहिए। उसे सतर्कतापूर्वक अपने मन को देखना चाहिए। उसे अपने वैराग्य, विवेक तथा जप एवं ध्यान का समय बढ़ा कर विकास करके कामनाओं को कलिकावस्था में ही नष्ट कर देना चाहिए।
उसे अखण्ड मौन ले लेना चाहिए और प्रबल ध्यान एवं प्राणायाम करना चाहिए। उसे ४० दिन तक दूध और फल पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। उसे गहन साधना में लग जाना चाहिए। कषाय का अर्थ है छुपी वासना। यह विषयासक्ति कहलाती है। सभी प्रकार की सांसारिक अभिलाषाएँ इसी में आती हैं। अभिलाषा मन को बहुत बेचैन कर देती है। मनुष्य को मात्र एक ही अभिलाषा से प्रेम होना चाहिए, वह है आत्म-साक्षात्कार ।
अध्याय ८
ध्यान में उच्च बाधाएँ
१. अभिलाषा एवं कामना
जब भी आपको कामना परेशान करे, तो विषयी जीवन के दोषों को देख कर वैराग्य प्राप्त करने का प्रयास करें। विषय-सुखों के प्रति वैराग्य का अर्जन कीजिए। सोचें कि सुख दर्द एवं विभिन्न परेशानियाँ उत्पन्न करता है तथा प्रत्येक वस्तु नाशवान् है। मन को विषयों से बार-बार वापस खींचें तथा इसे अमर आत्मा अथवा भगवान् के चित्र पर केन्द्रित करें। जब मन स्थिरता की स्थिति प्राप्त कर ले और जब यह विचलन तथा लय से मुक्त हो, तो इसे बाधित न करें।
आकांक्षित विषय, कामनाएँ तथा विभिन्न विघ्न डालने वाले विचार अन्य बाधाएँ हैं। विचार, इन्द्रियों के नियन्त्रण, वैराग्य, विवेक तथा ब्रह्मचर्य के द्वारा कामनाओं को नष्ट करें। योजना न बनायें। कल्पनाएँ न करें। उन्हें पूर्ण करने का प्रयास न करें। निरपेक्ष बने। आवेगों को दूर करें। कामनाओं में आसक्त न रहें। आवेगों तथा आसक्ति की अनुपस्थिति में कामनाएँ शक्तिहीन हो जाती हैं। वे दुर्बल हो जायेंगी और मर जायेंगी। विघ्न डालने वाले विचारों के कारण ढूँढ़ें और उन्हें एक-एक करके दूर करें। मन को सावधानीपूर्वक देखें। एकान्त में लीन हो जायें। किसी से घुलें मिलें नहीं। धैर्य, उत्साह और साहस रखें। यदि आपको ध्यान में अत्यधिक रुचि तथा आनन्द आये, यदि आप प्रगति कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए अध्ययन भी बन्द कर दें। अध्ययन भी एक विषय है। भगवान् किताबों में नहीं है। उसके पास निरन्तर ध्यान के द्वारा ही मात्र पहुँचा जा सकता है। समाज में प्रशंसा प्राप्त करना विद्वत्ता है। पाण्डित्य-प्रदर्शन छोड़ दें। कभी-कभी मन थकान का अनुभव करता है। तब पूर्ण विश्राम लें। मन पर जोर न डालें। सन्ध्या के समय समुद्र के किनारे, गंगा तट पर अथवा किसी अन्य रमणीक स्थल पर भ्रमण हेतु चले जायें। ॐ का उच्चारण करें। ॐ का अनुभव करें। ॐ का गान करें। दो-एक दिनों के लिए ध्यान का समय घटा दें। अपने दृढ़ सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें तथा अक्सर अपने भीतर से आने वाली आवाज को सुनें। मन की चित्तवृत्ति को अनुभव करें। हर्ष और शोक—ये दो तरंगें मन में घूम रही हैं। जब आप विषादग्रस्त हों, तो लम्बी दूरी तक घूमने के लिए चले जायें। किताबें बन्द कर दें। उत्कृष्ट विचारों पर विचार करें। अनुभव करें कि आप सर्व आनन्द हैं। स्मरण रखें कि ये सभी उपाधि के धर्म हैं और वे आत्मा से संयुक्त नहीं हैं। वे शीघ्र चले जायेंगे।
२. नैतिक और आध्यात्मिक अहंकार
जैसे ही साधक को कुछ आध्यात्मिक अनुभव होते हैं अथवा सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वह अज्ञानता एवं अहंकार से फूल जाता है। वह स्वयं के बारे में बहुत सोचता है। वह स्वयं को अन्यों से पृथक् कर लेता है। वह अन्यों के साथ अपमानजनक व्यवहार करता है। वह अन्यों के साथ घुल-मिल नहीं सकता। यदि किसी के भीतर कुछ नैतिक योग्यताएँ जैसे सेवा-भाव अथवा आत्म-त्याग अथवा ब्रह्मचर्य होगा, तो वह कहेगा- "मैं पिछले १२ वर्षों से अखण्ड ब्रह्मचारी हूँ। मेरे समान पवित्र कौन है? मैं पिछले ४ वर्षों से मात्र पत्तियों एवं चने पर जीवित हूँ। मैंने आश्रम में १० वर्षों तक सेवा की है। कोई भी मेरे समान सेवा नहीं कर सकता।" जिस प्रकार संसारी लोग सम्पत्ति के घमण्ड में फूल जाते हैं, उसी प्रकार साधु एवं साधक अपनी नैतिक योग्यताओं से फूल जाते हैं। इस प्रकार का अहंकार भी भगवद्-साक्षात्कार के मार्ग में भयंकर बाधा है। इसका पूर्णतया उन्मूलन किया जाना चाहिए। कोई मनुष्य जितना अधिक स्वयं की डींग हाँकता है, वह उतना ही अधिक क्षुद्र जीव मात्र है। उसके पास देवत्व नहीं होगा।
३. धार्मिक ढोंग (दम्भ )
जिस प्रकार संसारी लोगों में है, उसी प्रकार साधुओं में भी अनेक फैशन हैं। जिस प्रकार संसारी लोगों में ढोंग प्रचलित है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी निम्न प्रकृति को पूर्णतया शुद्ध नहीं किया है ऐसे साधकों, साधुओं एवं संन्यासियों में भी ढोंग उपस्थित होता है। वे जो वास्तव में नहीं होते है, वैसा दर्शाते हैं। वे बड़े महात्मा अथवा सिद्ध पुरुष की भाँति बैठते हैं, जब कि उन्हें योग अथवा आध्यात्मिकता का अक्षर-ज्ञान भी नहीं होता। वे कुछ ईसाई मिशनरियों के साथ सम्बन्ध रखते हैं और कभी-कभी छुट्टी के दिन एकत्रित भी होते हैं। यह खतरनाक वृत्ति है। वे अन्यों को छलते हैं। वे अपनी डींग हाँकते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं, बदमाशी करते हैं और सम्मान, अच्छा भोजन तथा वस्त्र प्राप्त करने तथा श्रद्धावान् मूर्खों को छलने के लिए ढोंग करते हैं। धर्म के व्यापार से बड़ा कोई पाप नहीं है। यह महान् पाप है। गृहस्थों को माफ किया जा सकता है; लेकिन हम साधकों और साधुओं को जो कि आध्यात्मिक पथ का अनुकरण कर रहे हैं तथा जिन्होंने भगवद्-साक्षात्कार के लिए सब-कुछ त्याग दिया है, उन्हें माफ नहीं कर सकते। धार्मिक ढोंग संसारी लोगों के पाखण्ड से अधिक खतरनाक है। इसके उन्मूलन के लिए लम्बे कठोर उपचार की आवश्यकता है। धार्मिक ढोंगी भगवान् से बहुत अधिक दूर है। वह भगवद्-साक्षात्कार का स्वप्न भी नहीं देख सकता। मोटे तिलक, माथे पर त्रिपुण्ड, तुलसी और रुद्राक्ष की अनेक मालाएँ गले, हार्थो, कलाइयों तथा कानों पर धारण करना—ये सभी धार्मिक ढोंग के कुछ बाह्य प्रतीक हैं।
४. कीर्ति और प्रतिष्ठा
मनुष्य अपनी पत्नी, पुत्र, सम्पत्ति आदि का भी त्याग कर सकता है; परन्तु कीर्ति और प्रतिष्ठा का त्याग करना कठिन है। आदर और सम्मान को कीर्ति और प्रतिष्ठा कहते हैं। यह भगवद्-साक्षात्कार के मार्ग में बड़ी बाधा है। यह अन्त में मनुष्य का अधःपतन करती है। यह साधक को आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर नहीं होने देती। वह मान तथा सम्मान का दास बन जाता है। साधक ज्यों ही थोड़ी चित्त-शुद्धि तथा नैतिक उन्नति प्राप्त करता है, त्यों ही अज्ञानी लोग उसके पास एकत्रित होने लगते हैं और उसको नमस्कार करते हैं तथा भेंट चढ़ाने लगते हैं। साधक अभिमान से फूल उठता है और सोचता है कि वह अब एक बड़ा महात्मा बन गया है। अन्ततः वह अपने प्रशंसकों का दास बन जाता है। वह अपने क्रमिक पतन को नहीं देख पाता। वह ज्यों ही गृहस्थों से मिलना-जुलना आरम्भ करता है, त्यों ही वह आठ दश वर्षों के तप काल में जो थोड़ा-बहुत प्राप्त किया था, उसे खो बैठता है। अब वह जनता को प्रभावित नहीं कर सकता और न ही लोगों को किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ ही पहुँचा पाता है। अन्त में उसके प्रशंसक भी उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी संगति में कोई सान्त्वना, शान्ति तथा आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं मिलती।
लोग ऐसा समझते हैं कि इस महात्मा के पास सिद्धियाँ हैं और वे उसकी कृपा से सन्तान तथा धन प्राप्त कर सकते हैं तथा रोगों का उपचार करवा सकते हैं। वे सदा ही विविध उद्देश्यों से साधु के पास जाते हैं। साधक कुसंगति में पड़ कर अपने वैराग्य तथा विवेक को खो बैठता है। आसक्ति तथा कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः साधक को सदा अपने को गुप्त रखना चाहिए। किसी को यह न मालूम हो कि वह किस प्रकार की साधना कर रहा है। उसे कभी किसी प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। उसे गृहस्थों से बहुमूल्य उपहार नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह उपहार देने वाले के बुरे विचारों से प्रभावित हो जायेगा। उसे आदर, मान, नाम तथा यश को विष्ठा अथवा विष के समान समझना चाहिए। अनादर तथा अपमान को अपना आभूषण बनाना चाहिए। तभी वह सुरक्षित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुँचेगा।
आश्रम बनाने तथा शिष्यों को दीक्षित करने से साधक का अधःपतन हो जाता है, क्योंकि इनसे कीर्ति और प्रतिष्ठा आती है। ये भगवद्-साक्षात्कार के मार्ग की बाधाएँ, हैं। साधक एक अन्य प्रकार का गृहस्थ बन जाता है। उसमें संस्थागत अहंकार विकसित होता है। उसकी आश्रम तथा शिष्यों में आसक्ति हो जाती है। आश्रम चलाने, पत्रिका मुद्रित करने तथा अपने शिष्यों को खिलाने के लिए वह वैसे ही ध्यान, चिन्ता तथा आकुलता रखता है जैसे गृहस्थ रखते हैं। उसमें दास-भावना आ जाती है तथा उसकी संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है। मरणासन्न अवस्था में आश्रम का विचार उसके मन में चक्कर काटता रहता है। कुछ महन्त अपने जीवन काल में आश्रमों को बहुत ही सुन्दर ढंग से संचालित करते हैं, किन्तु उनके महाप्रयाण के बाद उनके शिष्य जो कि संकीर्णमना होते हैं, परस्पर झगड़ते हैं। न्यायालयों में मुकदमे दायर होते हैं। तत्पश्चात् आश्रम लड़ाई के केन्द्र बन जाते हैं। आश्रम के स्वामियों को दानदाताओं से चिकनी-चुपड़ी बातें कहनी पड़ती हैं और प्रायः लोगों से कोष के लिए याचना करनी होती है। जो धन संचय तथा आश्रम के विकास में लगे हैं, उनके मस्तिष्क में ईश्वर-विषयक विचार भला कैसे रह सकता है? जिन्होंने आश्रम की संस्थापना की है, वे अब कहते हैं—“हम अनेक प्रकार से लोगों की भलाई कर रहे हैं। हम नित्य आध्यात्मिक कक्षाएँ चलाते हैं। हम गरीबों को भोजन देते हैं। हम निर्धन बालकों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। "
यह भी सत्य है कि जो आश्रम एक निष्काम योगी तथा साक्षात्कार प्राप्त जीवन्मुक्त द्वारा चलाया जाता है, वह आध्यात्मिकता का जाग्रत केन्द्र होता है। यह हजारों लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए आध्यात्मिक केन्द्र होता है। ऐसे केन्द्री की संसार के सभी भागों में आवश्यकता है। ऐसे आश्रम देश के लिए प्रचुर आध्यात्मिक कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आध्यात्मिक आश्रम जिनको चलाने वाले आध्यात्मिक प्रमुख हों, आजकल बहुत ही दुर्लभ हैं।
आश्रम के संस्थापक कुछ समय पश्चात् अचेतन रूप से दास बन जाते हैं। माया अनेक प्रकार से कार्य करती है। वे बड़े ही उत्सुक रहते हैं कि लोग उनका चरणामृत पियें। कोई भी मनुष्य जिसका ऐसा भाव है कि उसकी अवतार की भाँति पूजा की जाये, वह जनता की सेवा कैसे कर सकता है? कर्मचारी क्षुद्र बुद्धि वाले होते हैं। छोटे-छोटे विषयों पर उनके मध्य होने वाले झगड़े से आश्रम का वातावरण खराब होता है। तब आश्रम में शान्ति कहाँ होगी? आश्रम में आने वाले बाहरी लोग जो वहाँ शान्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं, वे वहाँ शान्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे।
आश्रम के संस्थापकों को नित्य बाहर से भिक्षा प्राप्त कर जीवन यापन करना चाहिए। उन्हें पूर्ण आत्म-त्याग का जीवन, आदर्श सादगी का जीवन जैसे कि ऋषिकेश के ब्रह्मलीन काली कमली वाला बाबा रहते थे, बिताना चाहिए। वे अपने आश्रम के लिए बाहर से जल का पात्र अपने सिर पर उठा कर लाते थे। वे बाहर से भिक्षा पर जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा करने पर ही मात्र वे लोगों का सही में कल्याण कर सकते हैं। आश्रम के संस्थापकों को कभी भी लोगों से दान हेतु याचना नहीं करनी चाहिए। जो भगवद्-साक्षात्कार के पथ का अनुकरण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐसा करना अपमानजनक है। यह अन्य प्रकार का सम्मानजनक भिक्षा माँगने का तरीका है। भीख माँगने की आदत बुद्धि की सूक्ष्म तथा संवेदनशील प्रकृति का नाश कर देती है तथा जो जल्दी-जल्दी दान माँगते हैं, वे नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार कि वकील तथा बदनाम लोगों के घरों में जाने वाले लोग असत्य में से सत्य, अपवित्रता में से पवित्रता खोजने की अपनी विवेक शक्ति खो बैठते हैं। बुद्धिमान् लोग धन एकत्र करने हेतु बुद्धिमानीपूर्ण विधियों का प्रयोग करते हैं। आजकल चोर भी बुद्धिमान होते हैं, वे मार्फिन का इंजेक्शन दे कर गाड़ियों में से धन चुरा लेते हैं। निम्न तरीका आधुनिक प्रकार का भिक्षा माँगने का तरीका है। एक बुद्धिमान् तथा पढ़ा-लिखा युवक रेल में चढ़ता है। उसके हाथ में कुछ रंग-बिरंगे कागज हैं। वह उन्हें यात्रियों में वितरित कर देता है। उसमें लिखा है- "मैं मैसूर के दीवान का पोता हूँ। मेरे पिता की अचानक मृत्यु हो गयी है। मेरी माँ की आयु ८५ वर्ष है। एक भाई गूँगा है। दूसरा भाई अन्धा है। कृपा करके थोड़ा धन दे कर मेरी सहायता करें।" यह आधुनिक प्रकार की भिक्षा है। वह कभी भी कटोरा या थाली ले कर भीख नहीं माँगता और न ही कोई बात करता है। लेकिन वह मुद्रित कागज बाँटता है। वह उत्तम पेंट-शर्ट पहनता है, टाई लगाता है और हैट पहनता है। वह थोड़ा धन एकत्र करता है। कागज वापस ले लेता है और शान्तिपूर्वक नीचे उतर जाता है और अगले डिब्बे में चला जाता है। भिक्षा आपके आत्म-बल को कम कर देती है। यह लोगों के मन पर गलत प्रभाव डालती है। यदि कोई भीख माँगता है, तो उसके लिए स्वतन्त्रता कहाँ है? लोग आश्रम के संस्थापकों में आस्था खो बैठते हैं। यदि बिना माँगे कोई चीज आती है, तो यह स्वीकार की जा सकती है। तब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ कार्य कर सकते हैं। वे गृहस्थ जो आश्रम चलाते हैं, वे दान माँग सकते हैं। आश्रम के लिए अच्छे कार्यकर्ता प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। जब न तो आपके पास धन है, न कार्यकर्ता है, न ही आध्यात्मिक शक्ति है, तो फिर आप आश्रम बनाने के लिए परेशान क्यों होते हैं? शान्त रहे। ध्यान करें। स्वयं का विकास करें। अपने काम से काम रखिए। पहले स्वयं का विकास कीजिए। आप दूसरों की सहायता कैसे कर सकते है, जब कि आप स्वयं अँधेरे में घिरे हैं और स्वयं ही अन्धे हैं? एक अन्धा आदमी दूसरे अन्धे को कैसे रास्ता दिखा सकता है? दोनों ही गहरी खाई में गिर जायेंगे तथा अपने पैर तोड़ डालेंगे।
शक्ति, नाम, कीर्ति तथा सम्पत्ति अहंकार को दृढ़ करते हैं। वे व्यक्तित्व को दृढ़ करते हैं। इसलिए यदि आप अमरता तथा अनन्त शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें त्याग दें।
अन्त में मैं वह बताना चाहता हूँ कि हमें वर्तमान में प्रथम श्रेणी के आश्रम नहीं मिलते, फिर भी यहाँ अच्छे द्वितीय श्रेणी के आश्रम हैं जो कि श्रेष्ठ सात्त्विक आत्माओं द्वारा चलाये जाते हैं, जो कि अनेक प्रकार से देश की महान् सेवा करते हैं, बहुमूल्य दार्शनिक पुस्तकें निकालते हैं और ध्यान तथा योग के अभ्यास में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं। वे निष्काम सेवा करते हैं। उनके कार्य वास्तव में प्रशंसा के लायक है। धनी लोगों का कर्तव्य है कि उन्हें धन तथा सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें। भगवान् उनको प्रेम, सेवा तथा शान्ति के सन्देश को फैलाने के लिए अन्तर आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें तथा उन दुर्लभ, श्रेष्ठ तथा निष्काम आत्माओं को मेरी मौन श्रद्धांजलि एवं प्रणाम !
५. भूत गण
ये भूत गण कभी-कभी ध्यानावस्था में दृष्टिगोचर होते हैं। इनका रूप विचित्र होता है—किसी के दाँत लम्बे, किसी का चेहरा बड़ा, किसी का पेट मोटा, किसी के पेट पर चेहरा, किसी के सिर पर मुख। ये सब भूतलोक के निवासी हैं। ये भूत हैं। ये सब भगवान् शिव के अनुचर माने जाते हैं। इनका रूप भयानक होता है। ये बिलकुल निरापद हैं। ये रंगमंच पर केवल दिखायी देते हैं। ये आपकी शक्ति और साहस परखने आते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नीतिवान्, चरित्रवान् साधक के सामने ये खड़े भी नहीं रह सकते। ॐ का जप उन्हें दूर फेंक देता है। आपको निर्भय रहना चाहिए। भीरु व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। सदा इस अनुभूति के द्वारा कि 'आप आत्मा हैं' साहस का विकास कीजिए। देह-भाव को अस्वीकार कीजिए। चौबीसों घण्टे निदिध्यासन कीजिए। यही रहस्य है। यही कुंजी है। यह सच्चिदान्द-रूपी कोष के द्वार को खोलने की कुंजी है। आनन्द-रूपी भवन की यह आधारशिला है। आनन्द के राजप्रासाद का यह प्रमुख स्तम्भ है।
६. दृश्य
दृश्य एवं अनुभव आते हैं और जाते हैं। वे साधना में स्वयं चरम सीमा नहीं हैं। जो इन छोटे-छोटे दृश्यों को बहुत अधिक महत्त्व देते हैं, वे आध्यात्मिक पथ में सहजता से नहीं चल सकते। इसलिए इन अनुभवों के विचार को त्याग दें। एकमात्र परमात्मा का अनुभव ही जो कि अन्त में अन्तः प्रेरित एवं प्रत्यक्ष होता है, वही एकमात्र सत्य है।
दृश्यों से ऊपर उठें। दृश्य जो आप ध्यान में देखते वे समाधि अथवा भगवद्-साक्षात्कार के मार्ग में बाधा हैं। जब आप उन्हें देखेंगे, तो मन भगवान् के स्थान पर सम्पूर्ण दिवस उन दृश्यों पर एकाग्र रहेगा। इन दृश्यों और उनके विचार की उपेक्षा करें, निरपेक्ष रहें और उनके स्थान पर भगवान् के विचार को प्रतिस्थापित करें।
७. सिद्धियाँ
नौ ऋद्धियाँ एवं आठ महत् सिद्धियाँ एवं अठारह छोटी सिद्धियाँ हैं। आठ सिद्धियाँ इस प्रकार है—अणिमा (अणु के आकार की), महिमा (विशालकाय), गरिमा (अत्यधिक भारी), लघिमा (अत्यन्त लघु), प्राप्ति (जिसकी भी कामना हो, उसकी प्राप्ति), प्राकाम्य (निर्बाध कामना), इशित्व (ईश्वरत्व) एवं वशित्व (प्रत्येक वस्तु पर नियन्त्रण) । ऋद्धि का अर्थ है समृद्धि। यह सिद्धि से निम्न है।
सिद्धियों के बारे में अधिक विचार न करें। दूर-दृष्टि तथा दूर-श्रवण का कोई महत्त्व नहीं है। उत्कृष्ट ज्ञान एवं शान्ति सिद्धियों के होने की अपेक्षा उनके बिना सम्भव है।
सिद्धियों के लिए कामना हवा के झोंके की भाँति है, जो योग के उस दीप को है, बुझा सकती है जो कि अत्यन्त सावधानीपूर्वक जलाया गया हो। भावना में कोई भी गिरावट होगी, तो वह असावधानी अथवा सिद्धियों के लिए स्वार्थपूर्ण कामना के कारण होगी। वह उस छोटी-सी आध्यात्मिक ज्योति को बुझा देगी जो कि योगी ने बड़े ही संघर्ष से प्रज्वलित की है तथा वह साधक को अज्ञानता की गहरी खाई में गिरा देगी। वह उस ऊँचाई तक पुनः नहीं पहुँच सकेगा, जहाँ वह पहले पहुँच गया था। प्रलोभन बस इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि साधक को किस प्रकार भ्रमित किया जाये। सूक्ष्म, मानसिक तथा गन्धर्व लोकों के प्रलोभन पृथ्वी के प्रलोभनों से अधिक शक्तिशाली होते. हैं।
जिस योगी ने अपनी इन्द्रियों, प्राण तथा मन को संयमित किया है, उसके पास अनेक सिद्धियाँ तथा अन्य शक्तियाँ स्वयं ही आती है। ये सब मार्ग के रोड़े हैं। वे योगाभ्यासी को प्रलोभित कर देंगी। साधकों को बड़ा ही सावधान रहना चाहिए और उन्हें सिद्धियाँ तथा अन्य शक्तियों को तुच्छ अथवा बेकार वस्तुओं की भाँति निर्दयतापूर्वक त्याग देना चाहिए।
यदि आप नियमित रूप से धारणा और ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो आपको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होंगी ही। आपको उन शक्तियों का प्रयोग तुच्छ एवं स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए, किसी प्रकार की भौतिक प्राप्ति हेतु नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपका पतन हो जायेगा। आपको माँ प्रकृति दण्ड देगी। क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। प्रत्येक गलत कर्म की प्रतिक्रिया होती ही है। मैं बार-बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ। सावधान रहें! शक्ति, स्त्री, धन तथा पाण्डित्य शक्तिशाली नशे की भाँति कार्य करते हैं। इनका धारक नहीं जानता कि वह वास्तव में क्या कर रहा है। उसकी बुद्धि कुन्द हो जाती है। उसकी समझ धुंधली हो जाती है। यदि आप यम के अभ्यास में • स्थित होंगे अथवा आत्म-संयमी होंगे, तो आप इन शक्तियों से प्रलोभित नहीं होंगे।
चमत्कार अथवा सिद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती। एक सामान्य आदमी उच्च आध्यात्मिक बातों के प्रति बिलकुल अज्ञानी रहता है। वह भुलावे की स्थिति में डूबा रहता है। वह उच्च परमोत्कृष्ट ज्ञान से अपरिचित रहता है, इस कारण वह अति सामान्य घटनाओं को अलौकिक मान बैठता है। एक योगी जो चीजों को योग के प्रकाश में समझता है, उसके लिए चमत्कार कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार गाँव का आदमी जब पहली बार एक हवाई जहाज अथवा एक बोलती पिक्चर देखता है, तो वह अवस्थित रह जाता है। उसी प्रकार सांसारिक मनुष्य जब पहली बार कोई अति सामान्य दृश्य देखता है, तो अचम्भित रह जाता है।
८. काषाय
काषाय आनन्द के द्वारा मन में उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म प्रभाव है तथा यह वही रह जाता है और यह समय-समय पर फलीभूत होता है और मन को समाधि से विचलित करता है। यह ध्यान में एक गम्भीर बाधा है। यह साधक को समाधि-निष्ठा में प्रवेश नहीं होने देता। यह उपभोग किये गये सुखों की सूक्ष्म स्मृति उत्पन्न करता है। यह गुप्त वासना है। संस्कार से वासना उत्पन्न होती है। संस्कार कारण है और वासना प्रभाव है। यह मल (मन की अशुद्धियों) का राजा है।
काषाय का अर्थ है रंगना। राग-द्वेष एवं मोह को काषाय अथवा मन को रंगना कहते हैं। ब्रह्म भावना के साथ संयुक्त का निरन्तर विचार करना ही इस भयंकर रोग काषाय की औषधि है।
९. लय
लय में मन जागता रहता है। यहाँ तक कि यदि आपने वैराग्य तथा ज्ञानाभ्यास अथवा ब्रह्म-चिन्तन के बार-बार अभ्यास द्वारा लय तथा विचलन को विजित कर लिया है, फिर भी मन पूर्ण सन्तुलन अथवा शान्त अवस्था में प्रवेश नहीं करता। यह एक मध्य अवस्था में रहता है। मन अभी भी राग से मुक्त नहीं हुआ है जो इसकी बाह्य विषयों की दिशा में इसकी सभी गतिविधियों का बीज है। अभी भी वासना अथवा गुप्त वासनाएँ और काषाय छुपी हुई है। आपको बार-बार विचार के द्वारा मन को संयमित करना होगा तथा कठोर ध्यान करना होगा तथा सम्प्रज्ञात अथवा सविकल्प समाधि का अभ्यास करना होगा। अन्त में आपको स्वयं को असम्प्रज्ञात अथवा (निर्बीज समाधि) में विश्राम देना चाहिए।
१०. रसास्वाद
रसास्वाद एक अन्य प्रकार का अनुभव है। यह वह आनन्द है जो निम्न सविकल्प समाधि में आता है। साधक जो इस परमानन्द का अनुभव करता है, वह कल्पना करता है कि वह अन्तिम लक्ष्य तक पहुँच गया है और वह साधना बन्द कर देता है। जिस प्रकार वह मनुष्य जो बहुमूल्य खजाने को खोजने के लिए जमीन को बहुत गहराई तक खोदता है, वह जमीन की सतह के नीचे प्राप्त होने वाली छोटी-मोटी चीजों से आकृष्ट नहीं होता, उसी प्रकार साधक को तब तक अपनी साधना करते रहनी चाहिए, जब तक वह भूमावस्था अर्थात् जीवन के परम लक्ष्य तक न पहुँच जाये। उसे अल्प अथवा निम्न अनुभवों से कभी सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे अपने अनुभवों से उपनिषदों में वर्णित सन्तों के उच्च अनुभवों की तुलना करनी चाहिए तथा देखना चाहिए कि वे वास्तव में उनसे मिलते-जुलते हैं या नहीं। उसे तब तक प्रयत्न करना चाहिए जब तक वह ज्ञान भूमिका तक न पहुँच जाये, ब्रह्मनिष्ठ न बन जाये उसे तब तक संघर्ष करना है जब तक उसे 'मैने सभी कामनाएँ प्राप्त कर ली है; मैंने सब कुछ कर लिया है; में सबकुछ जानता हूँ अब कोई चीज जाननी शेष नहीं है; अब कुछ भी और प्राप्त करना शेष नहीं है ऐसी आप्तकाम, कृतकृत्य तथा प्राप्तप्राप्य की आन्तरिक भावना न प्राप्त हो जाये ।
यह बाधा (रसास्वाद) साधक को सर्वोच्च निर्विकल्प आनन्द का उपयोग कर से रोकती है। विचार, विवेक, प्रार्थना, प्राणायाम, लगनशीलता तथा ध्यान में संघर्ष उपर्युक्त बाधाओं को दूर करते हैं।
११. तूष्णीभूत अवस्था
कभी-कभी मन थोड़े समय के लिए शान्त रहता है। आपके मन में न तो राग रहता है न द्वेष। मन की यह शान्त अवस्था तूष्णीभूत अवस्था कहलाती है। यह जाग्रतः अवस्था में उत्पन्न होती है। साधक इसे गलती से समाधि समझ लेता है। यह मन की उदासीन अवस्था है। यह भगवद्-साक्षात्कार के पथ में बाधक है। साधक को सावधानीपूर्वक अन्तरावलोकन तथा कठोर ध्यान द्वारा मन की इस अवस्था पर विजय पानी चाहिए। उसे इन अवस्थाओं पर नियन्त्रण पाने के लिए प्रभावकारी विधियाँ अपनानी चाहिए। मात्र पुस्तकों का अध्ययन उसकी अधिक सहायता नहीं कर सकेगा। अनुभव तथा अभ्यास उसका सच्चा कल्याण करेंगे।
१२. स्तब्ध अवस्था
स्तब्ध अवस्था अन्य प्रकार की मानसिक अवस्था है। भय अथवा आश्चर्य से यह अवस्था उत्पन्न होती है। यह तूष्णी अवस्था के समान है। यह भी पथ में एक अन्य बाधा है। जब आपको कोई स्तब्धकारी समाचार मिलता है, तो मन थोड़ी देर के लिए अचम्भित रह जाता है। यही स्तब्ध अवस्था है। तूष्णी एवं स्तब्ध ये दोनों ही वह अवस्थाएं है। यहाँ पूर्ण जागरूकता नहीं रहती। मन जड़ अवस्था में लकड़ी के लठ्ठे के समान रहता है। यह ध्यान हेतु अयोग्य हो जाता है। जब यह अवस्था उपस्थित रहती है. तो शरीर में भारीपन रहता है। मन उदास रहता है। उत्साह की कमी रहती है। मन भी कुछ समय के लिए उदास हो जाता है। इन लक्षणों से इस अवस्था को पहचाना जा सकता है एक बुद्धिमान् साधक जो नित्य ध्यान का अभ्यास करता है, यह उन विभिन्न अवस्थाओं को खोज निकालता है जिनमें मन जाता है। नवाभ्यासी को प्रारम्भ में ध्यान बड़ा शुष्क अनुभव होता है। लेकिन एक उच्च साधक जो मन की प्रकृति का तथा कार्यों और मानसिक ध्यान के नियमों का ज्ञान रखता है, उसे ध्यान बड़ा ही रुचिकर अनुभव होता है। जितना ही अधिक वह ध्यान करता है, उतना ही अधिक वह मन पर नियन्त्रण प्राप्त करता जाता है। वह वृत्तियों एवं विभिन्न मानसिक अवस्थाओं की प्रकृति को समझ सकता है। वह उनको नियन्त्रित कर सकता है। वह वास्तव में अनुभव करता है कि वह अन्तर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर रहा है तथा अब वह सरलतापूर्वक मन के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता।
१३. अव्यक्तम्
जब आप समाधि का अभ्यास करते हैं, तो अनेक विघ्न जैसे निद्रा, आलस्य, निरन्तरता में बाधा, भ्रम, प्रलोभन, सांसारिक सुखों के प्रति कामना तथा खालीपन का भाव आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। आपको सतर्क रहना होगा। आपको जागरूक तथा सतर्क होना चाहिए। आपको धैर्यपूर्वक निर्भयतापूर्वक प्रयासों के द्वारा पग-पग पर आने वाली इन बाधाओं को जीतना होगा। जब सभी वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, तो जो आपके सामने शून्य प्रकट होता है वह वास्तव में शून्य नहीं है। यह अव्यक्त है। इस शून्य को भी पार करें। यह आपको जीतने का प्रयास करेगा। अब आप अकेले रह गये हैं। आपके लिए अब सुनने तथा देखने को शेष नहीं है। आपको उत्साह देने वाला कोई नहीं है। आपको स्वयं पर निर्भर होना होगा। इस जटिल संगम पर चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। भीतर से साहस और शक्ति खींचें। उद्दालक ऋषि को इस शून्य को पार करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था।
उपसंहार
मेरे प्रिय साधको! मैं ऋषियों के धाम पवित्र हिमालय के शान्तिपूर्ण वातावरण से शान्ति की विचार-तरंगें भेजता हूँ।
भगवान् शान्तिस्वरूप हैं। श्रुतियों में प्रभावशाली कथन है। "अयं आत्मा शान्तः—यह आत्मा शान्त है।" कामना शान्ति की महान् शत्रु है। कामना अनेक प्रकार के विचलन करती है। जिसकी धारणा नहीं है, उसके लिए शान्ति नहीं है। अशान्त व्यक्ति के लिए कोई खुशी नहीं है। सभी दर्द, कष्ट और दुःख परम शान्ति में सदा के लिए नष्ट हो जायेंगे।
भाइयो! अमरता के पुत्रो! आगे बढ़ें, बढ़ते ही जायें। पीछे न देखे। भूतकाल को भूल जायें। शरीर और संसार को भूल जायें। केन्द्र को न भूलें। स्रोत को न भूलें। एक देदीप्यमान भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शुद्ध हो। सेवा करें। प्रेम करें। दान करें। ॐ में जियें । सर्वव्यापक उपस्थिति का सर्वत्र, सदैव अनुभव करें। अमरता के अमृत का पान करें। अन्तर्यामी की उपस्थिति आपका केन्द्र, आदर्श तथा लक्ष्य बने। आनन्द, खुशी, अमरता, शान्ति, कीर्ति, वैभव आपके साथ सदा के लिए रहें।
अमृतपुत्रो! मैंने आपके सामने उन सभी बाधाओं को विस्तार से रखा जो भगवद्-साक्षात्कार के मार्ग में खड़ी हैं तथा इन बाधाओं के उन्मूलन हेतु विभिन्न प्रभावशाली विधियाँ भी बतायी हैं। अब अजेय आध्यात्मिक योद्धा की तरह आध्यात्मिक युद्ध-क्षेत्र में खड़े हो जाइए। महान् निर्भीकता तथा अनूठे पराक्रम सम्पन्न आध्यात्मिक नायक बनें। निर्भय हो कर एक-एक करके सभी बाधाओं पर विजय पाइए तथा दैवी वैभव, कीर्ति, शुद्धता तथा साधुता को प्रकट करें। परिणामों के लिए शान्त तथा निश्चल मन के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जल्दबाज, अधीर तथा उतावले न बनें। आध्यात्मिक उत्थान तथा नवीनीकरण के लिए सही समय दें। कोई निराशा नहीं। वैराग्य के अस्त्र का बाना धारणा करें। विवेक की ढाल पहनें। आस्था की पताका धामे साहस तथा उत्साह के साथ 'भूम भूम भूम; ॐ ॐ ॐ; राम राम राम; श्याम श्याम श्याम' का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ें। जब तक हृदय भर कर अमरता का मधु न पी लें, तब तक रुकें नहीं, रुकें नहीं। प्रिय साधको! जब तक आप अनन्त सूर्यप्रकाश, अक्षय सौन्दर्य, कभी कम न होने वाले भावोन्माद, परमानन्द, अनन्त आनन्द, शुद्ध प्रसन्नता तथा अटूट शान्ति के अमर क्षेत्र में प्रवेश न कर लें, तब तक न रुकें। यह आपका अन्तिम गन्तव्य है। अब आप अनन्त शान्ति में विश्राम कर सकते हैं। यह आपका लक्ष्य है। यह आपका सर्वोच्च लक्ष्य तथा जीवन का उद्देश्य है। अब आप स्थायी शान्ति में विश्राम करें। मित्रो! आप सबको नमस्कार। स्वयं को दोष रहित करें। यह दुर्लभ रामबाण औषधि अपने भाइयों के साथ बाँटें। उनका उत्थान करें। यह श्रेष्ठ तथा विलक्षण निःस्वार्थ कर्म आपका विस्तृत योजना में प्रतीक्षा कर रहा है। दैवी इच्छा को पूर्ण कर तथा अक्षय प्रसिद्धि के बुद्ध बन जाइए। आप सबको प्रणाम।
जब किसी मधुमक्खी के पैर शहद में डूब जाते हैं, तो वह धीरे-धीरे अपने पैरों को चाट लेती है और आनन्दपूर्वक उड़ जाती है। इसी प्रकार मन के इस शरीर तथा बच्चों से राग और मोह के कारण चिपकने को वैराग्य और ध्यान के द्वारा रोके। इस मांस और हड्डी के पिंजड़े को छोड़ कर, स्रोत ब्रह्म अथवा परमात्मा की ओर उड़ जायें।
अब और कोई शब्द नहीं। बहुत हुए बहस और गर्म तर्क। एक शान्त कमरे में बैठें। आँखें बन्द करें। गहन शान्त ध्यान करें। उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। उनका नाम ॐ उत्साह, खुशी और प्रेमपूर्वक दोहरायें। अपना हृदय प्रेम से पूर्ण करें। संकल्पों, विचारों, मन की तरंगों, कल्पनाओं तथा कामनाओं को जब वे मन की सतह पर उठें, उसी समय नष्ट कर दें। घुमक्कड़ मन को वापस खींचें और इसे भगवान् पर केन्द्रित करें। ध्याननिष्ठा गहन और तीव्र हो जायेगा। अपनी आँखें न खोलें। अपने स्थान से न हिलें। उनमें लीन हो जायें। हृदय की अन्तरतम गुहाओं में गहरे गोते लगायें। देदीप्यमान आत्मा में भीतर लीन हो जायें। अमरता का मधु पियें। अब एकान्त का आनन्द लें। मैं अब आपको अकेला छोड़ता हूँ। अमृतपुत्रो, आनन्द करो! शान्ति, शान्ति! मौन! आप धन्य हैं, धन्य हैं!
अध्याय ९
ध्यान में अनुभव
१. ध्यान में विभिन्न अनुभव
१. ध्यान के प्रारम्भ में विभिन्न रंगों के प्रकाश जैसे सफेद, नीले, हरे तथा हरे और लाल रंग के प्रकाश का मिश्रण आदि मस्तक के सामने प्रकट होते हैं। ये सभी तन्मात्रिक प्रकाश हैं। प्रत्येक तत्त्व का अपना रंग है। पृथ्वी तत्त्व का रंग पीला है। जल तत्त्व का रंग सफेद है। अग्नि तत्त्व का रंग लाल है। वायु तत्त्व का रंग हरा है। आकाश का रंग नीला है। रंगीन प्रकाश इन तत्त्वों के कारण ही होते हैं।
कभी-कभी एक बड़ा सूर्य अथवा चन्द्रमा अथवा एक विद्युत् की भाँति चमक ध्यान के समय मस्तक के सामने प्रकट होती है। उन पर ध्यान न दें। उन्हें छोड़ दें। इन प्रकाशों के स्रोत में गहरे डूबने का प्रयत्न करें।
कभी-कभी देव, ऋषि, नित्य सिद्ध गण ध्यान में प्रकट होंगे। उनका आदरपूर्वक स्वागत करें। उन्हें प्रणाम करें। उनसे निर्देश प्राप्त करें। वे आपकी सहायता करने और आपको प्रोत्साहन देने के लिए प्रकट होते हैं।
धारणा एवं ध्यान के प्रारम्भ में आप मस्तक के मध्य में एक चमकदार तथा चकाचौंध करता हुआ प्रकाश देखेंगे। यह आधा या एक मिनट तक रहेगा और फिर अदृश्य हो जायेगा। यह प्रकाश ऊपर की ओर से या आसपास से चमक सकता है। कभी-कभी एक ६ या ८ इंच व्यास का सूर्य किरणों सहित या किरणों के बिना दिखायी देगा। आपको आपके गुरु या उपास्य की मूर्ति भी दिखायी दे सकती है।
जब आपको आत्मा की झलक प्राप्त हो , जब आपको चमकता प्रकाश दिखायी दे अथवा जब आपको कोई अन्य अतिविशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव हो, तो भयभीत न हों। साधना न त्यागें। उन्हें भूत न समझें। साहसी बनें। आनन्द के साथ साहसपूर्वक चलते रहें।
२. आपको किस प्रकार के स्वप्न आते हैं? जैसे ही आप जागते हैं, जब आप कमरे में अकेले रहते हैं या जब आप सड़क पर भ्रमण करते हैं, तो आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं? एक बन्द कमरे में जब आप ध्यान करते हैं तो आपके मन की जैसी स्थिति रहती है, क्या आप वही स्थिति सड़क पर भ्रमण करते समय भी बनाये रखते हैं? अन्तरावलोकन करें तथा मन को ध्यानपूर्वक देखें। यदि सड़क पर भ्रमण करते समय आपका मन व्याकुल होता है, तो आप अभी भी दुर्बल है। आप ध्यान में अधिक ऊपर नहीं पहुँचे हैं, आप आध्यात्मिकता में अभी आगे नहीं बढ़े हैं। ध्यान को प्रभावशाली ढंग से करते रहें। एक उच्च साधक को स्वप्न में भी ब्रह्म के विचार होने चाहिए।
मौन की शक्ति को समझें। मौन की शक्ति व्याख्यानों, वार्तालापों, धाराप्रवाह भाषणों तथा प्रवचनों से अधिक महान् है। भगवान् दक्षिणामूर्ति ने चार युवाओं— सनक, सनन्दन, सनातन एवं सनत्कुमार को मौन के द्वारा शिक्षा दी। मौन की भाषा भगवान् की भाषा है। मौन की भाषा हृदय की भाषा है। शान्त बैठें और मानसिक रूपान्तरणों को रोकें। शान्त बैठें और संसार को अन्तर आध्यात्मिक शक्ति भेजें। इससे सम्पूर्ण विश्व लाभान्वित होगा। शान्ति में जियें । शान्त बनें। मौन में विश्राम करें। आत्मा को जानें और मुक्त हो जायें।
जब आप प्रातःकाल ध्यान के लिए बैठें, अपना प्रेम और शान्ति सभी जीवित प्राणियों के लिए बाहर भेजें। कहें: “सर्वेषां शान्तिर्भवतु —सभी के लिए शान्ति हो; सर्वेषां स्वस्ति भवतु—सभी को समृद्धि प्राप्त हो; लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु – समस्त जगत् सुखी हो।”
शान्ति में सभी प्रकार के दर्द नष्ट हो जाते हैं, शान्त मनों वाले मनुष्यों की बुद्धि स्थिर बन जाती है। जब मानसिक शान्ति प्राप्त हो जाती है, तो इन्द्रिय-विषयों के प्रति कोई लालसा नहीं होती। योगी का उसकी बुद्धि पर पूर्ण नियन्त्रण होता है। बुद्धि आत्मा में निवास करती है। यह पूर्ण स्थिर रहती है। शरीर तथा मन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं।
ध्यान के समय आपके मन में समय का विचार नहीं होगा। आपको कोई ध्वनि नहीं सुनायी देगी। आपको वातावरण का कोई विचार नहीं होगा। आप अपना नाम तथा अन्यों के साथ सभी प्रकार के सम्बन्धों को भूल जायेंगे। आप शान्ति और आनन्द का उपभोग करेंगे। धीरे-धीरे आप समाधि में विश्राम करेंगे।।
प्रारम्भ में साधक आनन्द की अवस्था में थोड़े समय के लिए रहेगा। उसके बाद वह नीचे आ जाता है। अनवरत रूप से ध्यान के अभ्यास के द्वारा वह उत्कर्ष अवस्था में निरन्तर बना रहता है। बाद में देहाध्यास पूर्णरूपेण नष्ट हो जायेगा।
जब आप गहन ध्यान द्वारा शान्ति में प्रवेश करेंगे, तो बाह्य जगत् तथा आपकी कठिनाइयाँ समाप्त हो जायेंगी। आप परमानन्द का अनुभव करेंगे। इस शान्ति में ज्योतियों की परम ज्योति है। इस शान्ति में अक्षय आनन्द है। इस शान्ति में सच्ची शक्ति एवं आनन्द है।
जब आप कठोर ध्यानाभ्यास करेंगे, तो केवल कुम्भक स्वयं ही लग जायेगा। जब केवल कुम्भक लगेगा, आप प्रचुर शान्ति का अनुभव करेंगे तथा आपका मन एकाग्र होगा।
जो श्रुतियों में तथा स्मृति में बताये गये कर्तव्यों के प्रति निरन्तर समर्पित है तथा जो परब्रह्म को जानने हेतु प्रयत्नशील है, आत्मज्ञानी ऋषियों के दर्शन तथा अन्य अनुभवातीत विषय स्वयं ही उसके सामने आयेंगे। गहन ध्यान में पहले साधक बाह्य जगत् को भूलता है और बाद में शरीर को ।
ध्यान में ऊपर उठने का अनुभव एक चिह्न है जो संकेत करता है कि आप शरीर-चेतना से ऊपर उठ रहे हैं। जब आपको उपर्युक्त अनुभव होगा, उस समय आप एक विशेष प्रकार के आनन्द का अनुभव भी करेंगे। प्रारम्भ में यह ऊपर उठने वाला अनुभव एक मिनट तक ही रहता है। एक मिनट बाद आप अनुभव करेंगे कि आप पुनः सामान्य चेतना में वापस आ गये हैं।
आपको ध्यान के समय एक उच्च प्रकार की अवर्णनीय शान्ति का आनन्द प्राप्त होगा। लेकिन सच्चे आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त करने या अपने लक्ष्य (ध्यान के चुने हुए विषय) में मन को लीन करने में या शारीरिक चेतना से पूर्णतया मुक्त होने के लिए लम्बा समय लगता है। धैर्यवान् बनें। उद्यम करें। आप आगे बढ़ेंगे।
साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं में दैवी चेतना स्थायी है। यह प्रारम्भ में एक झलक की भाँति होती है। स्थिर ध्यान के द्वारा यह स्थायी अथवा स्वाभाविक बन जाती है।
३. मन को बाह्य अथवा आन्तरिक बिन्दु पर एकाग्र करना धारणा है। ध्यान के समय मन शान्त, निश्चल एवं स्थिर हो जाता है। मन की विभिन्न किरणें ध्यान के विषय पर एकत्रित एवं केन्द्रित होती हैं। मन लक्ष्य पर केन्द्रित हो जाता है। मन का यहाँ कोई विचलन नहीं होता, एक ही विचार मन को आपूरित किये रहता है। मन की सम्पूर्ण ऊर्जा एक ही विचार पर केन्द्रित रहती है। इन्द्रियाँ स्थिर हो जाती हैं। वे कार्य करना बन्द कर देती हैं। जब ध्यान गहन होता है, तो शरीर एवं आस-पास की कोई चेतना नहीं होती। जिसकी अच्छी धारणा होती है, वह भगवान् के चित्र को पलक झपकते ही बहुत ही स्पष्टता से देख सकता है।
अनावश्यक विचारों को भगाने का प्रयत्न न करें। जितना अधिक आप प्रयत्न करेंगे, उतना ही अधिक वे वापस आयेंगे तथा उतनी अधिक शक्ति प्राप्त करेंगे। वे आपकी ऊर्जा का अपव्यय करेंगे। निरपेक्ष बनें। मन को दैवी विचारों से भरें। वे धीरे-धीरे नष्ट हो जायेंगे।
ध्यानाभ्यास के समय सभी वृत्तियाँ अथवा मानसिक रूपान्तरण जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि सूक्ष्म रूप ग्रहण कर लेते हैं। वे तनु हो जाते हैं। वे समाधि अथवा ईश्वर के साथ पूर्ण मिलन के आनन्द के द्वारा ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाते हैं और तब आप पूर्ण सुरक्षित होंगे। छुपी हुई वृत्तियाँ बड़ा बृहत् रूप ग्रहण करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा में रहती हैं। आपको बड़ा ही सावधान तथा जागरूक रहना होगा।
जब आपका ध्यान गहन होगा, आपके शरीर की चेतना लुप्त हो जायेगी। आपको अनुभव होगा कि शरीर नहीं है। आपको प्रचुर आनन्द का अनुभव होगा। इस समय मानसिक चेतना होगी। कुछ लोग पहले पैरों में चेतना खो देते हैं, उसके बाद वे रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, वक्ष में तथा हाथों में चेतना खो देते हैं। जब इन अंगों में चेतना लुप्त हो जाती हैं, तो वे अनुभव करते हैं कि उनका सिर हवा में लटक गया है। मन शरीर की ओर वापस आने का प्रयत्न कर सकता है।
थोड़ी एकाग्रता अथवा मन की एकाग्रता को समाधि समझने की गलती न करें। चूँकि आप थोड़ी धारणा के कारण आप थोड़ा-सा ऊपर उठ गये हैं, तो इसे यह न समझ लें कि आपने समाधि प्राप्त कर ली है।
समाधि एक उच्च लक्ष्य है जिसे कोई भी मात्र ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकता है। यह वह चीज नहीं है जो थोड़े से अभ्यास से प्राप्त हो सके। समाधि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठोरता से ब्रह्मचर्य तथा आहार में नियमितता का पालन करना चाहिए तथा हृदय की शुद्धता होनी चाहिए। यदि इनका पालन नहीं किया गया, तो वह अवस्था प्राप्त करना सम्भव नहीं है। ये प्रारम्भिक योग्यताएँ अच्छी तरह अर्जित करनी चाहिए, तत्पश्चात् ही व्यक्ति को समाधि के प्रवेश-द्वार में प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई समाधि में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब कि वह भगवान् का महान् भक्त न हो, अन्यथा यह समाधि उसके लिए जड़ समाधि होगी।
समाधि की स्थिति वर्णनातीत है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए साधन अथवा भाषा नहीं है। यहाँ तक कि सांसारिक अनुभवों में भी आप जिसने सेब को न चखा हो, उसके समक्ष सेब फल का स्वाद नहीं अभिव्यक्त कर सकते। न ही आप रंग की प्रकृति एक अन्धे व्यक्ति को बता सकते हैं। सर्व आनन्द, शान्ति की स्थिति के लिए भी मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि व्यक्ति को इसका स्वयं ही अनुभव करना होगा।
जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे, संसार के विचार, वासनाएँ, अभिलाषाएँ आदि दब जायेंगी। यदि आप ध्यान में अनियमित रहेंगे तथा यदि आपका वैराग्य क्षीण हो गया है, तो वे पुनः प्रकट होने का प्रयत्न करेंगे। वे दृढ़ रहेंगे और विरोध करेंगे। इसलिए ध्यान में नियमित रहें तथा और कठोर साधना करें, और अधिक वैराग्य का अर्जन करें, वे धीरे-धीरे तनु हो जायेंगे और नष्ट हो जायेंगे।
आप संसार-सागर को ध्यान के द्वारा पार कर सकते हैं। ध्यान आपकी सभी दुःखों से रक्षा करेगा। इसलिए अपने ध्यान में नियमित रहें।
२. अनाहत ध्वनियाँ
अनाहत ध्वनियाँ वे रहस्यमय ध्वनियाँ हैं जो ध्यान के प्रारम्भ में योगी को सुनायी देती हैं। यह विषय नादानुसन्धान कहलाता है। यह प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों के शुद्धिकरण अथवा सूक्ष्म तरंगों के शुद्धिकरण का चिह्न है। ये ध्वनियाँ आपको अजपा गायत्री मन्त्र, 'हंसः सोहं' का एक लाख बार जप करने से भी सुनायी दे सकती हैं।
ये ध्वनियाँ कानों को बन्द अथवा खुले रखने पर दाहिने कान से सुनायी देती हैं। जब ये बन्द कान से सुनी जाती है, तो अधिक स्पष्ट होती हैं। कानों को योनिमुद्रा के द्वारा दोनों अंगूठों से बन्द कर लें। पद्म अथवा सिद्ध आसन में बैठ जायें। कानों को दोनों अँगूठों से बन्द कर लें और इन ध्वनियों को ध्यान से सुनें। कभी-कभी आपको बायें कान से भी ध्वनि सुनायी देगी। ध्वनि मात्र दाहिने कान से ही स्पष्ट क्यों सुनायी देती है? क्योंकि सूर्य नाड़ी (पिंगला) नासिका के दाहिनी ओर है। अनाहत ध्वनि ओंकार ध्वनि कहलाती है। यह हृदय में प्राण के स्पन्दन के कारण आती है।
ध्वनियों के दस प्रकार
जो नाद सुनायी देता है, वह १० प्रकार का होता है। प्रथम है चिनि, चिनि शब्द की तरह। दूसरा है चिनि-चिनि, तीसरी है घण्टी की ध्वनि, चौथी है शंख ध्वनि, पाँचवीं है तन्त्री (वीणा या सारंगी) ध्वनि, छठी है तबले की ध्वनि, सातवीं है वंशी की ध्वनि, आठवीं है भेरी (ढोल या नगाड़े) की ध्वनि तथा नौवीं है मृदंग की ध्वनि तथा दसवीं है बादलों की (गड़गड़ाहट) ध्वनि। जब तक आप अपने पैर को योग की सीढ़ी के रहस्यमय आवाजों के ऊपरी पायदान पर जमायेंगे, उसके पूर्व आपको अपने भीतरी भगवान् (परमात्मा) की आवाज सात प्रकार से सुनायी देगी। पहली है बुलबुल की वह मधुर आवाज जो यह अपने प्रिय से मिलने के लिए गाती है। दूसरी आती है ध्यानी जनों के चाँदी के झाँझ या मंजीरे की ध्वनि की तरह जो रुक-रुक कर आती है। अगली है समुद्री घोंघे का उसके खोल के भीतर बन्द रहने पर मधुर विलाप। इसके बाद वीणा की ध्वनि आती है। बाँसुरी की आवाज पाँचवीं है। इसके बाद अगली है दुन्दुभि की ध्वनि। अन्तिम ध्वनि है बादलों की गड़गड़ाती आवाज। सातवीं ध्वनि अन्य सभी ध्वनियों को लील जाती है। वे मृत हो जाती हैं। तब और कुछ सुनायी नहीं देता।
३. ध्यान में ज्योतियाँ
एकाग्रता के कारण ध्यान में अनेक प्रकार की ज्योतियाँ प्रकट होती है। एक चमकदार सफेद ज्योति एक बिन्दु की तरह मस्तक में त्रिकुटी (दोनों भौंहों के मध्य स्थान जो कि सूक्ष्म शरीर के आज्ञा चक्र से सम्बद्ध है) में प्रकट होती है।
आप देखेंगे कि जब आँखें बन्द होती हैं, तो विभिन्न रंगीन प्रकाश सफेद, पीला, लाल, धुएँ जैसा, नीला, हरा, मिश्रित प्रकाश, बिजली की तरह, अग्नि की तरह, जलते कोयले की तरह, या चन्द्रमा, सूर्य, तारे आदि की तरह चमकते हैं। ये प्रकाश चिदाकाश में प्रकट होते हैं। ये सभी तन्मात्रिक प्रकाश हैं। प्रत्येक तन्मात्रा का अपना रंग है। पृथ्वी तन्मात्रा का पीला प्रकाश है, जल तन्मात्रा का सफेद रंग का प्रकाश है। अग्नि तन्मात्रा का लाल रंग है, वायु तन्मात्रा का धुएँ जैसा प्रकाश है। आकाश तन्मात्रा का नीला प्रकाश कभी-कभी दिखायी देता है। सामान्यतया वहाँ श्वेत एवं पीला प्रकाश का संयुक्त रूप से दिखायी देता है। प्रारम्भ में मानसिक नेत्र के समक्ष श्वेत प्रकाश के छोटे-छोटे गोले तैरते हैं। जब आप पहली बार इसका अनुभव करें, तो निश्चय मानें कि मन अधिक स्थिर हो गया है तथा यह कि आप धारणा में प्रगति कर रहे हैं। कुछ माह पश्चात् प्रकाश का आकार बढ़ेगा तथा आप श्वेत प्रकाश की पूर्ण ज्वाला देखेंगे जो सूर्य से भी अधिक बड़ी होगी। प्रारम्भ में ये स्थिर नहीं रहेंगे। वे आयेंगे और तत्काल अदृश्य हो जायेंगे। ये मस्तक के ऊपर से तथा बाजू से चमकते हैं। ये अत्यधिक आनन्द तथा खुशी की विशेष संवेदना उत्पन्न करते हैं और इन प्रकाशों को देखने की तीव्र इच्छा होती है। जब आप दो या तीन घण्टे प्रातः काल तथा दो या तीन घण्टे रात्रि में नित्य नियमित और क्रमबद्ध अभ्यास करेंगे, तो ये प्रकाश जल्दी-जल्दी प्रकट होंगे तथा अधिक लम्बे समय तक स्थिर रहेंगे। प्रकाश का दृश्य साधना में महान् प्रोत्साहन है। यह आपको ध्यान में स्थिरता से लगने हेतु प्रेरित करेगा। यह पराभौतिक विषयों में दृढ़ विश्वास प्रदान करेगा। प्रकाश का प्राकट्य यह बताता है कि आप भौतिक चेतना से परे जा रहे हैं। जब प्रकाश प्रकट होता है, तो आप अर्ध चेतनावस्था में रहते हैं। इस समय आप दो धरातलों के मध्य हैं। आपको जब प्रकाश प्राप्त हो, तो अपने शरीर को नहीं हिलाना चाहिए। आपको आसन में शरीर को पूर्ण स्थिर रखना चाहिए। आपको अत्यन्त धीरे-धीरे श्वास लेनी चाहिए।
मुख-मण्डल में त्रिकोणी प्रकाश
जो भोजन मिताहारी है, जिसका क्रोध नियन्त्रित है, जिसने समाज के प्रति समस्त मोह त्याग दिया है, जिसने अपनी वासनाओं को विजित कर लिया है, जिसने सभी द्वन्द्वों पर विजय पा ली है, जिसने अपना अहंकार त्याग दिया है, जो न किसी को कुछ देता है न ही वह अन्यों से कोई चीज लेता है, ऐसा मनुष्य ध्यान के समय यह प्रकाश अपने मुख-मण्डल पर प्राप्त करता है।
सुषुम्ना से प्रकाश
“विशोका वा ज्योतिष्मती।” (अध्याय १, सूत्र ३६, पातंजल योग सूत्र) "जो सभी दुःखों से परे है, उस ज्योति पर ध्यान के द्वारा आप समाधि प्राप्त कर सकते हैं।"
कभी-कभी ध्यान के समय आप एक चमकदार प्रकाश देखेंगे। आपको इस प्रकाश पर दृष्टि टिकाना कठिन प्रतीत होगा। आप इस प्रकाश से अपनी मानसिक दृष्टि खींचने हेतु विवश हो जाते हैं। यह प्रकाश वह प्रकाश है जो हृदय में सुषुम्ना से निकलता है।
प्रकाश में रूप
आप दो प्रकार के रूप देखेंगे—१. देवताओं के आभामय रूप और २. शारीरिक रूप। आप अपने इष्टदेवता को सुन्दर वस्त्रों तथा विभिन्न बहुमूल्य आभूषणों, पुष्पों, मालाओं, चार हाथों एवं अस्त्रों सहित देखेंगे, सिद्ध गण तथा ऋषि गण आदि आपको प्रोत्साहित करने के लिए आयेंगे। आप उनके हाथ में बहुत से संगीत वाद्यों को देखेंगे। साथ ही आप स्वर्ग की अप्सराओं तथा देवताओं को देखेंगे। आप अनेक सुन्दर आकर्षक भवन, नदी, पहाड़, स्वर्ण मन्दिर, इतनी प्यारी और चित्रवत् दृश्यावलियाँ देखेंगे जिनका ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता।
चमकदार प्रकाश
ध्यान के समय कभी-कभी आपको अत्यन्त शक्तिशाली चमकदार प्रकाश प्राप्त होंगे जो सूर्य से भी अधिक बड़े होंगे। वे श्वेत रंग के होते हैं। प्रारम्भ में वे आते हैं और शीघ्र ही धुंधले पड़ जाते हैं। बाद में वे स्थिर हो जाते हैं तथा धारणा की शक्ति एवं स्तर के अनुरूप १० से १५ मिनट अथवा आधे घण्टे तक स्थिर रहते हैं। जो त्रिकुटी पर प्रकट होता है और जो सहस्रार चक्र पर सिर के शीर्ष भाग पर प्रकट होता है, वह प्रकाश इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि आप इस पर टिके नहीं रह सकते हैं और ध्यान छोड़ देते हैं। कुछ लोग डरते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं होता कि क्या करें और कैसे आगे बढ़ें। वे मेरे पास निर्देश हेतु आते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि यह एक नया संवेदन है जो उन्होंने पूर्व में कभी अनुभव नहीं किया। निरन्तर अभ्यास के द्वारा मन धारणा का अभ्यस्त हो जाता है और भय नष्ट हो जाता है। मैं उन्हें अभ्यास करते रहने के लिए कहता हूँ। कुछ हृदय पर धारणा करते हैं, कुछ त्रिकुटी पर और कुछ सिर के शीर्ष भाग पर। यह स्वयं की रुचि का प्रश्न है। त्रिकुटी पर धारणा के द्वारा मन को नियन्त्रित करना सरल होता है। यदि आपको त्रिकुटी पर धारणा करने की आदत है, तो सदा ऐसा ही करें। जल्दी-जल्दी परिवर्तन न करें। स्थिरता बहुत अधिक आवश्यक है। ध्यान की आरम्भिक अवधि में आप जिन प्राणियों तथा वस्तुओं से सम्बन्धित रहते हैं, वे सूक्ष्म जगत् से सम्बन्धित है। वे मानवों की भाँति हैं। उनमें शरीर का आवरण नहीं है। जिस प्रकार मानवों में कामनाएँ, आकांक्षाएँ, प्रेम, घृणा आदि होते हैं, ठीक उसी प्रकार उनमें भी ये सब होते हैं। उनका शरीर सूक्ष्म है। वे उन्मुक्तता से भ्रमण कर सकते हैं। उनमें उत्पादन, विनाश, बहुगुणित होना, दूर-दृष्टि आदि की थोड़ी सामर्थ्य होती है। ज्योतिर्मय रूप मानसिक एवं उच्च लोकों के उच्च देवताओं का है, जो आपको दर्शन देने के लिए तथा आपको प्रोत्साहित करने के लिए आये हैं। जब वे आपको दर्शन दें, तो आप उनकी मानसिक पूजा करें। देवदूत मानसिक अथवा उच्च लोकों के प्राणी है। वे आपके मानसिक नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे।
जब आप वास्तव में भौतिक शरीर से दबावपूर्वक नये लोक में प्रवेश करेंगे, तो कभी-कभी आपको सम्भवतया आपके इष्टदेवता की ओर से एक अदृश्य सहायता का अनुभव होगा। यह अदृश्य शक्ति आपको शरीर से अलग होने में तथा शारीरिक चेतना से ऊपर जाने में सहायता करेगी। आपको इन सभी क्रिया-विधियों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना होगा।
इन दृश्यों को देखने में समय न बरबाद करें। यह मात्र एक उत्सुकता है। ये सभी आपको पराभौतिक आध्यात्मिक सत्यता एवं ब्रह्म के ठोस अस्तित्व से सहमत कराने हेतु प्रोत्साहन हैं। इन दृश्यों को हटा दें। स्वयं को लक्ष्य पर दृढ़ करें। आगे बढ़ें। गम्भीरतापूर्वक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें।
जैसे ही आप निद्रा हेतु लेटेंगे, ये प्रकाश आपके बिना किसी प्रयत्न के स्वयं को प्रकट करेंगे। ठीक उस समय जब आप शारीरिक चेतना को पार करेंगे, जब आप तन्द्रा में होंगे, ये प्रकाश स्वयं ही बिना आपके किसी प्रयास के प्रकट होंगे। इसी प्रकार प्रातःकाल भी सुबह जागने के पूर्व, जब आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे होंगे, अर्ध निद्रा और अर्ध जाग्रत अवस्था में होंगे, तब भी बिना किसी प्रयत्न के आप पुनः उन प्रकाशों को पायेंगे।
कभी-कभी ध्यान के समय आप एक अनन्त नीला आकाश, पारलौकिक स्थान देखेंगे। आप स्वयं को नीले ब्रह्माण्ड में एक काले बिन्दु की तरह देखेंगे। कभी-कभी आपका रूप प्रकाश के केन्द्र में प्रकट होगा। कभी-कभी आप उच्च स्पन्दनयुक्त घूमते हुए कणों को प्रकाश में देखेंगे। आप भौतिक रूप, मानव रूप, बच्चे, स्त्री, प्रौढ़ पुरुष, दाढ़ी वाले ऋषि गण, सिद्ध तथा तेजोमय रूप देखेंगे। दृश्य अवास्तविक अथवा वास्तविक होंगे। ये आपकी स्वयं की मानसिक दृष्टि अथवा पदार्थों के सूक्ष्म लोक की यथार्थता के हो सकते हैं। विश्व विभिन्न स्तरों में विभिन्न लोकों से निर्मित है। तन्मात्रा के सामंजस्य पूर्ण स्पन्दन विभिन्न स्तरों में विभिन्न लोकों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक लोक में उसकी वस्तुएँ और प्राणी हैं। ये दृश्य वे वस्तुएँ या प्राणी हो सकते हैं। वे शुद्ध काल्पनिक भी हो सकते हैं। वे आपके स्वयं के तीव्र विचार का क्रिस्टलीकरण हो सकते हैं। योग-साधना में आपके पास विवेक होना चाहिए। सर्वत्र बुद्धि एवं सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
४. साधकों के रहस्यमय अनुभव
"तीन वर्ष पूर्व मुझे अपने सूर्य प्रतान में ध्यान के समय विशेष संवेदना का अनुभव हुआ। मुझे एक घूमते हुए चक्र का अनुभव हुआ। इसके बाद मुझे कुछ विशेष दृश्य दिखायी दिये। मैंने अपनी आँखों से चारों तरफ लोगों के सिर तथा इमारतों की सतह पर नीला तथा सफेद प्रकाश देखा। जब मैंने दिन के समय खुले विस्तृत आकाश की ओर देखा, तो एक कीड़े जैसी सफेद ज्योति इधर-उधर जा रही थी। जब मैं अपने कार्यालय में कार्य कर रहा था, तो मेरी आँखों के सामने सफेद चमकदार प्रकाश दिखायी दिया। कभी-कभी प्रकाश की छोटी-छोटी किरणें मेरी पुस्तकों पर दिखायी दीं। इसने मुझे एक विशिष्ट आनन्द दिया और मैं भगवान् का नाम गाने लगा 'श्री राम जय राम जय जय राम ।' आजकल जब मैं साइकिल से आफिस जाता हूँ, तो एक गोल गेंद की तरह प्रकाश दिखायी देता है और जब तक मैं अपने गन्तव्य तक नहीं पहुँच जाता, तब तक दिखायी देता रहता है। जब मैं सुन्दर आकाश की ओर देखता हूँ, यही चीज उस समय भी दिखायी देती है।”. "स.' "
"मैंने गंगोत्री में एक माह के लिए नित्य ५ घण्टे ध्यान किया। एक दिन मुझे तनिक भी शान्ति नहीं मिल रही थी। मुझे मन का उचाट होना सहन नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं गंगा तट पर बैठ गया और महात्मा गान्धी पर ध्यान करने लगा। इसने मुझे शान्ति प्रदान की। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मैं श्री राम जी पर आधे घण्टे तक ध्यान करता रहा। यह सगुण ध्यान अपने आप निर्गुण ध्यान में परिवर्तित हो गया। मुझे १० मिनट तक पूर्ण शान्ति का अनुभव हुआ। मेरा मन ॐ पर ध्यान में पूर्णतया लीन हो गया। यह आधे घण्टे तक चलता रहा। एक दिन मुझे विभिन्न प्रकार का अनुभव हुआ। मैंने ध्यान के बाद आँखें खोल लीं। मैंने बुद्धि की सहायता के बिना प्रत्येक चीज को ब्रह्म की भाँति अनुभव किया, मुझे यही अनुभव दिन-भर रहा। एक ब्रह्मचारी ने मुझसे उस दिन १ घण्टे बातें कीं। मैं मात्र उसकी बातें सुन रहा था, किन्तु मेरा मन उसकी बातों में नहीं था। वह उसी भाव में था। मैं उसका एक शब्द भी याद नहीं रख सका।
“अन्य अवसर पर मैंने आधे घण्टे ध्यान किया। मैं बड़े ही भावातिरेक में था, लेकिन बाहर से आती हुई कुछ ध्वनियों से यह भावावेशित मन विचलित हो गया। मैं पुनः ध्यान करने लगा। मैंने अपने हृदय के नीचे से एक सुन्दर प्रकाश देखा। जैसे ही वह प्रकाश अदृश्य हो गया, मैं अनजाने ही रोने लगा। कोई मेरे पास आया और उसने मेरा नाम ले कर पुकारा। मुझे कुछ ध्यान नहीं था। उसने मेरे शरीर को हिलाया। मैंने थोड़ा रोना बन्द कर दिया और उसके चेहरे की ओर देखा और पुनः २५ मिनट तक रोता रहा।"............. "व."
"मैंने पहली बार दिनांक २६-२-३२ से ४-२-३२ तक मौन रखा।"
“गलतियाँ” – कभी-कभी मैंने अपने विचार अंग-संचालन द्वारा व्यक्त किये। अन्तिम तीन दिनों मैंने 'हाँ', 'पर्याप्त' और 'क्या' शब्द अनजाने ही बोले। मुझे यह गलत कल्पना थी कि मेरे जबड़ों में दर्द है। मुझे बोलने हेतु बड़ी उत्कण्ठा थी।
“लाभ” – मैं अधिक काम करने लगा, अधिक स्वाध्याय करने लगा और जप तथा ध्यान सामान्य से अधिक समय तक करने लगा। मैं अर्धरात्रि के पूर्व सो ही नहीं पाता था। पुस्तकों के विचार मध्य रात्रि तक मेरे मन में घूमते रहते थे। क्रोध तथा चिड़चिड़ाहट बिलकुल नहीं थी। मैं किसी भी चीज को स्मरण नहीं रख पाता था। मैंने कुछ श्लोकों को याद करने का प्रयास किया, लेकिन न कर सका। ऐसा इसलिए, क्योंकि मेरी जोर-जोर से बोल बोल कर याद करने की आदत थी।"....." राम.
“मैंने एक माह तक प्राणायाम किया और मुझे कुछ मधुर ध्वनियाँ अथवा नाद जैसे वंशी, वायलिन, घण्टी, मृदंग, शंखध्वनि, तबले की ध्वनि, तूफान की आवाज कभी-कभी दाहिने कान से तथा अन्य समय दोनों कानों से सुनायी देने लगी।” ....... "न. "
"धारणा के समय मुझे कुछ अतिविशिष्ट सुगन्ध आने लगी।' " ;;;;र"
“मैं ध्यान के समय अपनी त्रिकुटी पर एक चमकदार सूर्य या चमकदार प्रकाश या एक सितारा देखता हूँ। यह दृश्य स्थिर नहीं रहता।”...... "ग.
“मैं अक्सर ध्यान के समय त्रिकुटी पर कुछ ऋषियों के दर्शन करता हूँ। मैं अक्सर अपने इष्ट कृष्ण को हाथों में मुरली लिये देखता हूँ।”....... "स. "
“मैं अक्सर ध्यान के समय त्रिकुटी में लाल, हरा, नीला और सफेद प्रकाश देखता हूँ। मैं स्वयं नीले आकाश में एक बिन्दु के रूप में प्रकट होता हूँ।".
“ध्यान के समय में अक्सर कई देवताओं तथा देवियों को तेजोमय शरीर एवं आभूषण धारण किये हुए देखता हूँ।".
“कभी-कभी ध्यान के समय मैं अक्सर एक बड़ा शून्य मात्र देखता हूँ।”.....“ट.”
“ध्यान के समय मैं अक्सर अपना ही मुख एक बड़े प्रकाश के केन्द्र में देखता हूँ । अक्सर मैं अपने मित्रों के चेहरे देखता हूँ। मैं स्पष्टतया उन्हें पहचान सकता हूँ।”.....“र.”
"मैं जब ध्यान हेतु बैठता हूँ, तो मूलाधार से गर्दन के पीछे तक विद्युत् सी दौड़ती अनुभव होती है। सामान्य समय में भी मुझे इसका अनुभव होता है।"......... "क. "
"ध्यान के समय कुछ सूक्ष्म अस्तित्व वाले, जिनके भूत के समान चेहरे एवं लम्बे दाँत हैं, काले रंग के अक्सर आ कर मुझे डराते हैं; लेकिन वे कोई हानि नहीं- करते।”. ............"न.'
"जब मैं ध्यान हेतु बैठता हूँ, तो अक्सर मुझे हाथों और पैरों में झटकों का अनुभव होता है। कभी-कभी मेरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद जाता है। " ..... ''इ''
"मैं अक्सर आँखें खुली रख कर ध्यान करता हूँ। एक रात को मैंने अपने सामने चमकदार प्रकाश देखा। उस प्रकाश के केन्द्र में मैंने भगवान् कृष्ण को हाथों में बाँसुरी लिये देखा। मेरे रोयें खड़े हो गये। मैं मूक हो गया। मैं आश्चर्य से भौंचक्का रह गया। यह प्रातःकाल ३ बजे का समय था।"....... "स."
"एक दिन मैं गहन ध्यान में था। मैंने स्वयं को वास्तव में भौतिक शरीर से पृथक् कर लिया। वास्तव में इसे केंचुली की भाँति देखा। यह हवा में तैर रहा था। मुझे अत्यधिक आनन्द और अत्यधिक भय की विशिष्ट संवेदना हुई। मैं दो-एक मिनट के लिए हवा में स्थिर रहा। महान् भय के कारण मैं अचानक भौतिक शरीर के भीतर वापस प्रवेश कर गया। मैं भौतिक शरीर के भीतर धीरे-धीरे एक विशेष संवेदना के साथ उतर रहा था। यह अनुभव रोमांचकारी था। ".....' "स. "
ऋषि उद्दालक का अनुभव
ऋषि उद्दालक समाधि (जो कि व्यक्ति को सत्य के आनन्दपूर्ण लोक में प्रवेश कराती है) नहीं लगा पाते थे; क्योंकि उनका मन बन्दर के समान तेजी से इन्द्रिय-विषयों की एक शाखा से अन्य शाखा पर कूदता था। वे पद्मासन में बैठते थे और प्रणव (ॐ) का उच्चारण जोर से किया करते थे। उसके बाद वे अपना ध्यान प्रारम्भ किया करते थे।
उन्होंने बलपूर्वक अपने मन पर नियन्त्रण किया। बड़ी ही कठिनाई से उन्होंने इन्द्रियों को विषयों से पृथक् किया। उन्होंने स्वयं को सभी बाह्य विषयों से असम्बद्ध कर लिया। उन्होंने शरीर के सभी द्वारों को बन्द कर लिया। उन्होंने अपने मन को हृदय पर केन्द्रित किया। उनका मन सभी विकल्पों से मुक्त हो गया। उन्होंने विषयों के सभी विचारों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया, जिस प्रकार एक योद्धा अपनी तलवार से अपने विरुद्ध बार-बार उठने वाले शत्रुओं को मार डालता है।
उनको अपने सामने एक तेज प्रकाश दिखा। उन्होंने मोह को अदृश्य कर दिया। उन्होंने अन्धकार, प्रकाश, निद्रा और मोह की अवस्था को पार किया। वे निर्विकल्प समाधि में पहुँच गये और पूर्ण शान्ति का आनन्द लिया। ६ माह पश्चात् वे अपनी समाधि से जागे। वे एक साथ दिनों, मार्हो तथा यहाँ तक कि वर्षों तक गहन समाधि में बैठे रहते थे और फिर समाधि से जागते थे।
५. ध्यान के क्षणों में
ब्रह्म आत्मा, पुरुष, चैतन्य, चेतना, भगवान्, अमरता, मुक्ति, पूर्णता, शान्ति, आनन्द, भूमा अथवा सहज समानार्थी शब्द हैं। यदि आप एक आत्म-साक्षात्कार ही मात्र प्राप्त कर लें, तो आप जन्म-मृत्यु के चक्रों तथा इसके पापों से मुक्त हो जायेंगे। जीवन का उद्देश्य है अन्तिम लक्ष्य अथवा मोक्ष प्राप्त करना। जो निष्काम सेवा, जप आदि द्वारा शुद्ध और स्थिर हो, ऐसे हृदय पर निरन्तर ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
यथार्थता अथवा ब्रह्म का साक्षाकार मात्र मनुष्य ही कर सकता है। अनेक लोगों ने आत्म-साक्षात्कार प्राप्त किया। अनेकों ने निर्विकल्प समाधि का आनन्द लिया। शंकर, दत्तात्रेय, मंसूर, शम्स तबरेज, ईसामसीह, बुद्ध आदि सभी साक्षात्कार प्राप्त आत्माएँ र्थी, जिनको सत्य अथवा दिव्य दृष्टि अथवा अपरोक्षानुभूति थी। लेकिन जो उन्होंने जाना, वह अन्यों को बताना सम्भव नहीं है। आप मिश्री का स्वाद उसे नहीं बता सकते, जिसने कभी इसे चखा न हो। आप रंग का विचार उसे नहीं बता सकते, जिसने उसे कभी देखा न हो। गुरु मात्र इतना ही कर सकता है कि वह अपने शिष्य को सत्य या वह मार्ग जो अन्तर्दृष्टि की क्षमता को अनावृत करे, को जानने की विधि बता सकता है।
ये वे चिह्न हैं जो यह संकेत करते हैं कि आप ध्यान में तथा ईश्वर के पास पहुँचने में विकास कर रहे हैं। आपको संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहेगा। इन्द्रिय-विषय आपको और अधिक न प्रलोभित करेंगे। आप कामना रहित, निर्भय, '३' रहित तथा 'मेरा' रहित बन जायेंगे। देहाध्यास अथवा शरीर के प्रति मोह धीरे-धीरे नष्ट हो जायेगा। आप 'वह मेरी पत्नी है', 'वह मेरा पुत्र है, 'वह मेरा घर है' आदि विचारों का पोषण नहीं करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि सभी भगवान् के प्रकट रूप है। आप प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का दर्शन करेंगे।
शरीर तथा मन हल्के हो जायेंगे। आप सदा उत्साहित और प्रसन्न रहेंगे। ईश्वर का नाम सदा आपके होठों पर होगा। मन सदा भगवान् के चरणों पर केन्द्रित रहेगा। मन सदा भगवान् का चित्र बनाता रहेगा। वह सदा भगवान् के चित्र के दर्शन करेगा। आप वास्तव में अनुभव करेंगे कि सत्त्व अथवा शुद्धता, प्रकाश, आनन्द, ज्ञान तथा प्रेम सदा भगवान् की ओर से आपकी ओर प्रवाहित हो रहे हैं और आपके हृदय को आपूरित कर रहे हैं।
आपको कोई शारीरिक चेतना नहीं होगी। यदि वहाँ शारीरिक चेतना होगी भी, तो यह मानसिक स्मृति के रूप में होगी। एक शराबी को उसके शरीर पर कपड़ा है, इस बात की पूर्ण चेतना नहीं रहती। वह अनुभव कर सकता है कि कोई चीज उसके शरीर पर ढीली-ढीली लटक रही है। इसी प्रकार आपको शरीर का अनुभव होगा।
आप अनुभव करेंगे कि कोई चीज आपसे एक ढीले कपड़े या ढीले जूते की तरह चिपकी हुई है।
आपको लिंग के प्रति कोई आकर्षण न होगा। आपको लिंग का कोई विचार न होगा। स्त्री आपके समक्ष प्रभु के प्राकट्य के रूप में प्रकट होगी। रुपये और सोना आपको पत्थर के टुकड़े की भाँति प्रतीत होंगे। आपको सभी प्राणियों के प्रति अत्यधिक प्रेम होगा। आप वासना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, मोह आदि से पूर्ण मुक्त होंगे। यहाँ तक कि लोग यदि आपका अपमान करेंगे, आपको मारेंगे या परेशान करेंगे, तो भी आपका मन शान्त होगा। इसका कारण यह है कि आपने अन्तर्यामी अथवा भगवान् से प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है, इसी कारण आप व्यग्र नहीं हो रहे हैं। दुःख-सुख, सफलता-असफलता, मान-अपमान, आदर अनादर, हानि-लाभ आपके लिए एक समान होंगे।
स्वप्न में भी आप भगवान् के सम्पर्क में रहेंगे। आप कोई सांसारिक चित्र नहीं देखेंगे।
आप प्रारम्भ में भगवान् के साथ बातें करेंगे। आप उन्हें शारीरिक रूप में देखेंगे। जब आपकी चेतना दैवी हो जायेगी, वार्तालाप बन्द हो जायेगा। आप मौन की भाषा अथवा हृदय की भाषा का आनन्द लेंगे। बैखरी से आप मध्यमा, पश्यन्ति, परा (ध्वनि के सूक्ष्म रूप) तक जायेंगे और अन्त में आप निशब्द ओंकार या निशब्द ब्रह्म में विश्राम करेंगे।
वैराग्य तथा विवेक, निर्मलता, आत्म-संयम, मन की एकाग्रता, अहिंसा, सत्य, पवित्रता, धैर्य, सहिष्णुता, सहनशीलता, दयालुता, क्रोध की अनुपस्थिति, सेवा का भाव, त्याग, सभी के प्रति प्रेम आपके स्वाभाविक गुण होगे। आप विश्व के मित्र तथा उपकारी होंगे।
ध्यान के समय आपको समय का विचार नहीं होगा। आपको कोई ध्वनि सुनायी नहीं देगी। आपको वातावरण का कोई विचार न होगा। आप अपना नाम तथा अन्यों के साथ सभी सम्बन्ध भूल जायेंगे। आप पूर्ण शान्ति और आनन्द का अनुभव करेंगे। धीरे-धीरे आप समाधि में स्थित हो जायेंगे।
समाधि एक अवर्णनीय अवस्था है। यह मन और वाणी के परे है। समाधि में ध्यान करने वाला अपनी वैयक्तिकता खो देता है और परमात्मा के साथ एक हो जाता है। वह आनन्द, शान्ति तथा ज्ञान का मूर्तिमान रूप बन जाता है। बस, इतना ही कहा जा सकता है। आपको निरन्तर ध्यान के द्वारा इसका स्वयं ही अनुभव करना होगा।
सन्तोष, मन की अविचल अवस्था, उत्साह, धैर्य, मल-मूत्र में कमी, मधुर वाणी, ध्यानाभ्यास हेतु उत्कण्ठा और स्थिरता, सांसारिक सम्पत्ति, सफलता और साथ हेतु अरुचि, एक अकेले कमरे अथवा एकान्त में रहने की इच्छा, साधुओं और संन्यासियों के साथ रहने की इच्छा तथा मन की एकाग्रता ये वे चिह्न हैं जो कि यह इंगित करते हैं कि आप शुद्धता में विकास कर रहे हैं तथा यह कि आप आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ रहे हैं।
आपको ध्यान के समय विभिन्न प्रकार के अनाहत नाद जैसे घण्टी की आवाज, नगाड़े की आवाज, तूफान की आवाज, शंख, वीणा या वंशी की ध्वनि, मधुमक्खी का गुंजन आदि सुनायी देंगे। मन इनमें से किसी एक पर एकाग्र हो जायेगा। यह भी समाधि की ओर प्रेरित करता है। आप ध्यान के समय विभिन्न प्रकार के प्रकाश एवं ज्योतियाँ देखेंगे। यह लक्ष्य नहीं है। आपको मन को उस स्रोत में लीन करना है जो इनका स्रोत है।
वेदान्त के मार्ग का अनुयायी इन ध्वनियों और प्रकाशों की उपेक्षा करता है। वह सभी रूपों की उपेक्षा के द्वारा उपनिषदों के महावाक्यों के महत्त्व पर ध्यान करता है। "वहाँ सूर्य नहीं चमकता; न तारे, न चन्द्रमा ही चमकते हैं, न यह विद्युत् ही चमकती है, तो इस अग्नि की बात ही क्या है? जब वह चमकता है, तो हर चीज उसके बाद चमकती है।” वह इस प्रकार ध्यान करता है—“वहाँ वायु नहीं बहती, अग्नि वहाँ नहीं जलती है। उस एक सार में न ध्वनि है न स्पर्श, न ही गन्ध न रंग, न मन न प्राण हैं। अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अगन्ध, अप्राण, अतीन्द्रिय, अदृश्य, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं आनन्दपूर्ण शिव हूँ, मैं आनन्दपूर्ण शिव हूँ।"
आध्यात्मिक युद्ध-क्षेत्र में आध्यात्मिक नायक बनें। एक बहादुर, अजेय आध्यात्मिक योद्धा बनें। मन, इन्द्रियों, वासनाओं तथा संस्कारों के साथ आन्तरिक युद्ध बाह्य युद्ध से अधिक भयंकर है। मन, इन्द्रियों, बुरी वासनाओं, तृष्णाओं, वृत्तियों तथा संस्कारों के विरुद्ध बहादुरी से युद्ध करें। मन को प्रभावकारी ढंग से उड़ाने के लिए ब्रह्म-विचार की मशीनगन का प्रयोग करें। गहरे गोते लगायें और वासना, लोभ, घृणा, अहंकार और ईर्ष्या की अन्तर तरंगों को 'ॐ' अथवा 'सोऽहं' के जप की तोप से नष्ट कर दें। आत्मा के आनन्द के उच्च लोकों में ब्रह्माकार-वृत्ति के हवाई जहाज की सहायता से ऊँचे उड़ें। अवचेतन मन के समुद्र में छिपी वासनाओं को उड़ाने के लिए ॐ के जप की तोपों का प्रयोग करें। कभी-कभी अपने दस शत्रुओं, दस उपद्रवी इन्द्रियों को कुचलने के लिए विवेक के टैंकों को चलायें। दिव्य संस्थाएँ प्रारम्भ करें और अपने शक्तिशाली मित्रों जैसे वैराग्य, सहनशीलता, निश्चलता, धैर्य, आत्म-संयम आदि को अपने शत्रु मन को नष्ट करने के लिए मित्र बनायें। शरीर के भव्य भवन तथा 'मैं शरीर हूँ', 'मैं कर्ता हूँ', 'मैं आनन्द लेने वाला हूँ, इन विचारों को नष्ट करने के लिए 'शिवोऽहं' भावना का बम डालें। आपके आन्तरिक शत्रुओं— रजोगुण तथा तमोगुण को शीघ्र नष्ट करने के लिए 'सत्त्व' की गैस छोड़ें। मन को वृत्तियों एवं संकल्पों या इन्द्रिय-विषयों के सभी बल्बों को निकाल कर रिक्त करें, जिससे कि मन शत्रु आप पर आक्रमण न कर सकें। आत्मिक मोती के बहुमूल्य खजाने पर कब्जा रखने के लिए एकाग्रता की बन्दूक का अपने शत्रु मन के विरुद्ध प्रयोग करें। समाधि तथा मोक्ष के आनन्द, निर्वाण की शान्ति अब आपकी है। चाहे आप कोई भी हों, चाहे आपने किसी भी जाति में जन्म लिया हो, चाहे आपका पिछला कोई भी जीवन या इतिहास हो, अपनी मुक्ति को प्राप्त करें। हे प्रिय राम! उपर्युक्त साधनों की सहायता से अभी, इसी क्षण विजय प्राप्त करें!
६. भगवान् का दर्शन
आप कभी-कभी एक बड़ी चमकदार स्वर्णिम ज्योति देखेंगे। इस प्रकाश के भीतर आप अपने इष्टदेवता को देखेंगे। कभी-कभी आप स्वयं को प्रकाश के भीतर देखेंगे। आप अपने चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश देखेंगे।
आप अपने इष्टदेवता को सूर्य की भाँति चमकते हुए पहाड़ जितना बड़ा देख सकते हैं। आप यह रूप भोजन करते हुए तथा काम करते हुए देखेंगे। जब आप इस दृश्य के आनन्द को ले रहे होंगे, तो आपको भोजन का कोई स्वाद नहीं आयेगा। आप बस भोजन को निगल लेंगे। आप निरन्तर वीणा बजने का स्वर सुनेंगे। आप सूर्य का चमकदार प्रकाश देखेंगे।
यदि आप नियमित ध्यान का अभ्यास करेंगे, आपके ध्यान का विषय आपके सामने शीघ्र आयेगा। आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि सम्पूर्ण अन्तरिक्ष प्रकाशित हो गया है। कभी-कभी आप बजती हुई घण्टियों की ध्वनि को सुनेंगे। आप आत्मा की आन्तरिक शान्ति का अनुभव करेंगे।
आप सभी प्रकार के सुन्दर रंगों को देखेंगे। कभी-कभी आप आकर्षक दृश्यावली के साथ एक सुन्दर बगीचा देखेंगे। कभी-कभी आप सन्तों और ऋषियों को देखेंगे। पूर्ण चन्द्र, अष्टमी का चाँद, सूर्य तथा तारे प्रकट होंगे। आप दीवार पर प्रकाश देखेंगे।
जब आपको ये अनुभव होंगे, जब आप ये दृश्य देखेंगे, तो आपको एक विशिष्ट प्रकार के अवर्णनीय आनन्द का अनुभव होगा। मिथ्या सन्तुष्टि न प्राप्त करें। ये सोच कर कि आपने सर्वोच्च साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, अपनी साधना और ध्यान को न रोकें। इन दृश्यों को अधिक महत्त्व न दें। आपको मात्र प्रथम श्रेणी की धारणा प्राप्त हुई है। सर्वोच्च लक्ष्य अथवा साक्षात्कार वह परम शान्ति है जहाँ सभी विचार रुक जाते हैं और आप परमात्मा के साथ एक बन जाते हैं।
वह जो जप, प्राणायाम तथा ध्यान करता है, उसे शरीर के हलकेपन का अनुभव होता है। रजोगुण तथा तमोगुण कम हो जाते हैं। शरीर हलका जाता है।
ध्यान में अचानक झटके विशेषकर तब आते हैं जब प्राण धीमा हो जाता और बाहर के स्पन्दन मन को इसके ईश्वर के साथ मिलन से नीचे भौतिक चेतना के स्तर को ले कर आते हैं।
मन जप, कीर्तन, ध्यान तथा प्राणायाम के अभ्यास से बहुत सूक्ष्म बन जाता है। विचार की शक्ति भी विकसित हो जाती है। आप ध्यान के समय ॐ की मधुर ध्वनि सुनेंगे। आप अपने गुरु का रूप देखेंगे।
आप अन्तिम लक्ष्य अथवा अनन्त वैभव तथा स्थायी शान्ति के अवर्णनीय ब्रह्म स्थान को निरन्तर ध्यान द्वारा प्राप्त करें।
७. पृथकता का अनुभव
अभ्यास के समय एक दिन आप अनुभव करेंगे कि आपने स्वयं को शरीर पृथक कर लिया है। आपको प्रचुर आनन्द के साथ मिश्रित भय का अनुभव होगा। एक नये हल्के सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति का आनन्द तथा विदेशी अनजाने लोक में प्रवेश के कारण भय का अनुभवा आरम्भ में एक नयी चेतना नवे लोक में अत्यधिक अल्प विकसित होगी, ठीक उसी प्रकार जैसे एक बच्चा जिसने अभी अभी आँखें खोली हैं। आपको मात्र ऐसा अनुभव होगा जैसे आपका शरीर वायु के समान हलका है तथा एक घूमता, स्पन्दित सीमित सूक्ष्म वातावरण है जिसमें आप स्वर्णिम ज्योतियाँ, विषय, प्राणी आदि देखेंगे। आप अनुभव कर सकते हैं कि आप वायु में घूम रहे हैं या तैर रहे हैं तथा इसके कारण आपको गिरने का भय होगा।
आप कभी भी गिरेंगे नहीं, बल्कि प्रारम्भ में एक सूक्ष्मता के नये अनुभव से नवी भावनाएँ तथा प्रारम्भ में संवेदन उत्पन्न होंगे। आप शरीर कैसे छोड़ेंगे, यह आरम्भ में अज्ञात रहेगा। जब आप पूर्णतया अलग हो जायेंगे तथा आप जब नये लोक में प्रवेश करेंगे, आप अचानक भौंचक्के रह जायेंगे। कभी-कभी चारों ओर नीले रंग का घेरा, तो कभी-कभी आंशिक प्रकाश के साथ मिश्रित अन्धकार तथा अन्य समय अत्यधिक चमकदार स्वर्णिम पीले रंग का प्रकाश बिखरा हुआ होगा। इस नवीन आनन्द को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकेगा, यह अवर्णनीय होगा। आपको स्वयं ही वास्तव में अनुभव करना होगा और आपको स्वयं ही खाना होगा। आप इससे अनभिज्ञ रहेंगे कि आप कैसे शरीर छोड़ेंगे, लेकिन आप अपनी वापसी के प्रति पूर्ण चैतन्य रहेंगे। आपको धीरे से अनुभव होगा कि आप बड़ी ही चिकनी सतह पर उतर रहे हैं, जैसे कि आप बड़े ही धीमे से किसी पतली नली के छोटे से छेद में से एक वायु के समान हल्के शरीर के साथ प्रवेश कर रहे हैं। आपको एक वायु के समान अनुभव होगा। जिस प्रकार वायु एक खिड़की की दरारों में से प्रवेश करती है, उसी प्रकार आप नवीन सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं सोचता हूँ कि मैंने विचार को स्पष्टतया व्यक्त किया है। जब आप वापस आयेंगे, तो आप जीवन को स्थूल एवं सूक्ष्म धरातल में भिन्नता कर सकेंगे। वहाँ नवीन चेतना को पुनः प्राप्त करने और उस अवस्था में सदैव रहने की तीव्र अभिलाषा होगी। आप नवीन लोक में ३, ५ या १० मिनट से अधिक रहने योग्य नहीं होंगे। बाद में आप अपनी इच्छानुसार कठिनाई से अपना शरीर त्याग सकेंगे। प्रारम्भ में प्रयासों के द्वारा आप साधना के समय माह में एक बार शरीर को पृथक् कर सकेंगे। यदि आप धैर्य, अध्यवसाय तथा दृढ़ता के साथ बढ़ेंगे, तो आप इच्छानुसार शरीर छोड़ सकेंगे और नवीन सूक्ष्म शरीर के साथ नवीन लोक में अधिक लम्बे समय तक रह सकेंगे आप शरीर के साथ एकता भाव रखने के विरुद्ध पूर्ण सुरक्षित होंगे। आपने देहाध्यास पर विजय प्राप्त कर ली है। जब आप नवीन लोक में २ या ३ घण्टे के लिए रह सकेंगे, तो ही आपकी स्थिति सुरक्षित होगी, इसके सिवा नहीं। मौन, एकान्त, अकेले रहना इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु रामबाण औषधि है। यदि परिस्थितियाँ आपको मौन रखने से रोकें, तो लम्बी बातचीत, सभी अनावश्यक वार्तालाप, सभी व्यर्थ की बहस आदि की कठोरता से उपेक्षा करें एवं यथासम्भव समाज से स्वयं को अलग कर लें। अत्यधिक बातचीत से मात्र ऊर्जा व्यर्थ होती है। यदि यह ऊर्जा मौन द्वारा संरक्षित रखी जाये, यदि इसे ओज अथवा आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपान्तरित किया जाये, तो यह आपकी साधना में सहायता करेगी। बागी छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार वाक् तेजोमय है। अमि का बड़ा भाग हड्डी के निर्माण में जाता है। मध्य भाग मज्जा बनाता है तथा सूक्ष्म भाग वाणी बनाता है। इसलिए वाणी अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा है। इस बात का स्मरण रखें। ३ माह, ६ माह अथवा १ वर्ष का मौन का पालन करें। यदि आप ऐसा निरन्तर महीनों तक न कर सकें, तो सप्ताह में एक दिन करें, जिस प्रकार महात्मा गान्धी जी ने किया था। आपको महात्माओं जैसे श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो अभी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में गंगा के उद्गम गंगोत्री में कई वर्षों से नंगे बदन रह रहे हैं। उन्होंने अनेक वर्षों से काष्ठ मौन ले रखा है (काष्ठ मौन में आप अपने विचारों को अन्यों को लिख कर अथवा संकेत के द्वारा भी व्यक्त नहीं करते) । आप भी महत् आदर और सम्मान वाले श्री कृष्ण आश्रम क्यों नहीं बन जाते? निरन्तर कठोर साधना से आप स्वयं को शरीर से अत्यन्त शीघ्र अलग कर सकेंगे। इसकी एक आदत स्थापित हो जायेगी। जितनी शीघ्र आप विचारों को शान्त कर सकेंगे तथा मन को शान्त करेंगे, उतनी ही शीघ्र भौतिक शरीर से यान्त्रिक रूप से निकलने की मानसिक आदत बन जायेगी। तब वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। मन नवी गलियों में प्रवेश करेगा तथा एक नवी अवस्था अथवा नवीन लोक में प्रकट होगा।
सूक्ष्म जगत् की यात्रा
आप सरलता से इच्छा मात्र से ही जहाँ चाहे सूक्ष्म शरीर द्वारा (सूक्ष्म लोक की) यात्रा कर सकते हैं तथा वहाँ अस्मिता (अहंकार) अथवा विश्व कोष से (तन्मात्राओं के समुद्र से) आवश्यक पदार्थों को खींच कर वहाँ निर्मित हो सकते हैं। यह क्रिया-विधि योगियों के लिए अत्यन्त सरल है, क्योंकि वे बुद्धिसम्पन्न हैं तथा विभिन्न क्रिया-विधियों की विस्तृत तकनीक जानते हैं। लेकिन यह नश्वर प्राणी जो कि भावनाओं तथा वासनाओं और मोहयुक्त होते हैं, के लिए अति विशिष्ट है। जो सूक्ष्म शरीर से कार्य कर सकते हैं, वे अत्यन्त सरलतापूर्वक विचार पठन तथा विचार प्रेषण करते हैं। एकाग्र मानसिक किरणें दीवारों में भी प्रवेश कर सकती हैं, जिस प्रकार एक्सरे किरणें हड्डियों से गुजर सकती हैं।
भौतिकीकरण
जीवात्मा का साक्षात् प्रकट होना या दिखायी देना
सर्वप्रथम आप संकल्प मात्र से स्वयं को शरीर से अलग करेंगे, उसके बाद आप स्वयं को मन से एक करेंगे, तब आप मानसिक लोक में इस सूक्ष्म शरीर से उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं, जिस प्रकार आप इस भूलोक में करते हैं। धारणा के द्वारा आप शरीर की चेतना से ऊपर उठ जायेंगे। ध्यान के द्वारा आप मन से ऊपर उठ जायेंगे तथा अन्त में आप ब्रह्म के साथ एक बन जायेंगे। अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ये तीन महत्त्वपूर्ण अन्तरंग साधनाएँ हैं।
८. दैवी चेतना
यह उत्कृष्ट आनन्द पूर्ण अनुभव, अन्तर्ज्ञान अथवा समाधि से आता है। निम्न मन बाह्य विषयाश्रित जगत् से वापस खींच लिया जाता है। इन्द्रियाँ मन से असम्बन्धित हैं। जीवात्मा का मन दैवी मन या हिरण्यगर्भ या विश्व की आत्मा या एक ही सूत्रात्मा के साथ एक हो जाती है। योगी जीवित आत्मा बन जाता है तथा अपने नये दैवी ज्ञान के द्वारा चीजों के जीवन में देखता है।
दैवी चेतना अवस्था बृहत् और श्रेष्ठ है। यह वर्णनातीत है। मन तथा वाणी इससे चकरा कर वापस आ जाती है, क्योंकि वे इसे ग्रहण करने तथा इसका वर्णन करने में सक्षम नहीं होतीं। वाणी एवं शब्द अपूर्ण हैं। यह परमानन्द तथा उच्च शुद्ध आनन्द जो कि दर्द, दुःख तथा भय से मुक्त है, को प्रेरित करती है। यह कारण जगत् का प्रकटीकरण है जहाँ प्रकारों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है।
श्री शंकर, दत्तात्रेय, वामदेव, तुलसीदास, जड़भरत, कबीर, हाफिज, तुकाराम, मदालसा, याज्ञवल्क्य, रामदास, मंसूर, शम्स तबरेज, मीरा, गौरांग, माधवाचार्य, रामानुचार्य, प्रभु ईशु, भगवान् बुद्ध, भगवान् मोहम्मद, भगवान् जोरोस्टर ने देवी चेतना का अनुभव किया था।
वह योगी जिसने देवी चेतना का अनुभव किया है, उसके पास सभी देवी ऐश्वर्य होते हैं। उसे अनेक प्रकार की सिद्धियाँ जिनका श्रीमद्भागवत तथा पतंजलि महर्षि के राजयोग में वर्णन किया गया है. प्राप्त होती है।
अर्जुन, संजय तथा यशोदा ने दैवी चेतना को अनुभव किया था। यशोदा ने बालकृष्ण के मुख में सम्पूर्ण विश्व के दर्शन किये थे।
गीता ने इन शब्दों में अर्जुन के मुख से दैवी चेतना की अवस्था का वर्णन किया है—‘“आपका विशाल रूप अनेक मुख तथा नेत्रों, दीर्घ भुजाओं, असंख्य जाँचों और पैरों के सहित है, आपका विशाल वक्षस्थल, अनेक भयंकर दाँत हैं तथा आपका सौन्दर्य चकाचौंध कर देने वाला है। आप स्वर्ग को स्पर्श कर रहे हैं। आपका इन्द्रधनुषी रंग है। आप खुले मुखों तथा चारों ओर चमकदार बृहत् नेत्रों के साथ सभी को निगल रहे हैं। भयंकर जीभों से युक्त आप अपने मुखों में मनुष्य जाति को निकलते जा रहे हैं। आपके जो कि भयंकर दाँतों वाले हैं, वे देखने में भयंकर हैं। वे अनेक सिर जो मुख आपके दाँतों के मध्य की जगह में पकड़े गये हैं, चूर्ण-चूर्ण हुए जा रहे हैं और पीसे जा रहे हैं।
फ्रांस में प्रोफेसर बर्गसन ने अन्तर्ज्ञान के बारे में शिक्षा के परे है, लेकिन इसके प्रतिकूल नहीं है। जो कि बुद्धि की पहुँच
यह नवीन अनुभव नवीन ज्ञान प्रदान करता है, जो अनुभवकर्ता को अस्तित्व का नया लोक प्रदान करता है। वहाँ उल्लास तथा अवर्णनीय आनन्द तथा प्रसन्नता का अवर्णनीय अनुभव है। वह वैश्विकता का अनुभव अनन्त जीवन की चेतना का अनुभव करता है। यह मात्र कल्पना नहीं है। वह वास्तव में इसको अनुभव करता है। उसे दिव्य नेत्र प्राप्त हो गये हैं।
जीवत्व अब चला गया है। क्षुद्र मैं पिघल गया है। भेद मन जो विभाजित करता है, वह नष्ट हो गया। सभी विघ्न, द्वैत के सभी भाव, भेदभाव, पृथकता का भाव अदृश्य हो गया है। समय व स्थान का कोई विचार नहीं है। वहाँ मात्र अनन्तता है। जाति, पथ, रंग के विचार अब चले गये। उसे आप्तकाम (जिसने वह सभी प्राप्त कर लिया है, जिसकी उसने कामना की है) भाव होता है। वह अनुभव करता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो मुझे जाननी चाहिए। उसे ज्ञान के परम चैतन्य लोक की पूर्ण जागरूकता तथा अन्तःप्रेरणा का अनुभव होता है। वह सृष्टि का सम्पूर्ण रहस्य जान जाता है। वह सर्वज्ञ है। वह सर्वविद् अथवा सृष्टि के समस्त विवरण का ज्ञाता है।
पूर्ण निर्भयता, निष्कामता, निर्विचारता, मैं रहितता, मेरापन का अभाव, क्रोध का न होना, चेहरे के चारों ओर ब्रह्मतेज का आभा-मण्डल, हर्ष एवं शोक से मुक्ति आदि कुछ चिह्न हैं, जो यह बताते हैं कि वह व्यक्ति परम चेतनावस्था तक पहुँच गया है। वह सदा पूर्ण आनन्द की अवस्था में रहता है। आप क्रोध, हताशा, हतोत्साह तथा दुःख उसके मुख पर कभी नहीं देखेंगे। आप उसकी उपस्थिति में उत्थान, खुशी और शान्ति पायेंगे।
दैवी चेतना जीवन की एकता की पूर्ण जागरूकता है। योगी अनुभव करता है कि विश्व एक ही जीवन से पूर्ण है। वह वास्तव में अनुभव करता है कि अन्धे बल अथवा मृत पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं है और यह कि सभी जीवित स्पन्दित तथा बुद्धिमान् हैं। यह वैज्ञानिक बोस का भी अनुभव है। उन्होंने इसे प्रयोगशाला के प्रयोगों के द्वारा प्रदर्शित किया।
जिसके पास दैवी चेतना होती है, वह अनुभव करता है कि सम्पूर्ण विश्व उसका है। वह परम प्रभु के साथ एक है। वह विश्व ज्ञान एवं जीवन के साथ एक है। वह उस आनन्द और खुशी का अनुभव करता है, जो समझ तथा वर्णन के परे है। ज्ञान अथवा महान् आध्यात्मिक उत्कर्ष के क्षणों में उसे वास्तविक वैश्विक दिव्य दृष्टि रहती है। वह भगवान् की उपस्थिति में चैतन्य रहता है। वह भगवान् के मुख के प्रकाश को देखता है। वह चैतन्यता के सामान्य धरातल से ऊपर उठ जाता है। उसे दिव्य या वैश्विक बुद्धि होती है। उसने दिव्य अनुभूति का विकास कर लिया है। मानव-आत्मा में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाता है।
उसे मृत्यु अथवा भविष्य अथवा वर्तमान शरीर के जीवन के रुकने के बाद क्या होगा, इसकी चिन्ता नहीं होती। वह नित्यता, अनन्तता तथा अमरता से एक हो जाता है।
ज्ञान के समय आनन्द के बाँध टूट जाते हैं। योगी अवर्णनीय भावोन्माद की लहरों से आप्लावित हो जाता है। आनन्द, अमरता, नित्यता, सत्य, दैवी प्रेम उसके व्यक्तित्व का अंश, उसके जीवन का सार बन जाते हैं। उसके जीवन का सार एकमात्र सम्भव सत्यता है। वह स्वीकार करता है कि आनन्द का स्थायी झरना प्रत्येक के हृदय में रहता है, वह अमर जीवन सभी प्राणियों में रहता है, यह अनन्त, सभी को गले लगाने वाला, सर्वव्यापक प्रेम प्रत्येक कण-कण को प्रत्येक अणु को आवृत करता है, सहारा देता है तथा निर्देशन करता है। सृष्टि के प्रत्येक अणु पाप, दुःख, मृत्यु आदि का अब उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। वह अनुभव करता है कि जीवन का सार, अमरता का अमृत उसकी नसों में प्रवाहित हो रहा है।
वह भोजन अथवा निद्रा की कोई आवश्यकता का अनुभव नहीं करता। वह पूर्ण निष्काम है। उसके व्यक्तित्व एवं तरीकों में महान परिवर्तन होता है। उसका मुख मण्डल तेज से दमकता है। उसके नेत्र तेजोमय रहते हैं। वह अनुभव करता है कि सम्पूर्ण जगत् सन्तुष्ट करने वाले प्रेम अथवा अमर आनन्द के समुद्र में स्नान कर रहा है, जो कि जीवन का सार है।
सम्पूर्ण जगत् उसके लिए उसका घर है। उसे कभी भी कोई भी स्थान अनजाना नहीं लगता। पहाड़ तथा दूसरे प्रदेश जिनको उसने कभी देखा भी नहीं, वह उसके अपने हो जाते हैं जैसे कि वे उसके अपने घर हों। वह अनुभव करता है कि सम्पूर्ण जगत् उसका शरीर है। वह अनुभव करता है कि सारे हाथ, सारे पैर उसके हैं।
थकान उसके लिए अनजानी है। उसके काम जैसे बच्चों का खेल है आनन्द तथा चिन्ता से रहित। वह सर्वत्र मात्र ईश्वर को देखता है। उसके लिए कुर्सी, टेबल तथा पेड का देवी महत्त्व है। कभी-कभी उसकी श्वास पूर्णतया रुक जाती है। वह परम शान्ति का अनुभव करता है। समय तथा स्थान नष्ट हो जाते हैं।
देवी चेतना सभी पुरुषों तथा स्त्रियों की अन्तर्निष्ठ स्वाभाविक योग्यता है। प्रशिक्षण तथा संयम चेतना को जगाने हेतु आवश्यक हैं। यह मनुष्य में स्वभावतः उपस्थित है। यह अधिकांश मानवों में अज्ञान के कारण अक्रियाशील है।
आप सभी अपने जन्मसिद्ध अधिकार, केन्द्र, आदर्श, लक्ष्य उस दैवी चेतना की स्थिति को ऋषियों, पवित्रता, प्रेम, शक्ति तथा ज्ञान के साथ संयोग के द्वारा प्राप्त करें।
९. आनन्दमय अनुभव
समाधि या परमानन्दपूर्ण दैवी अनुभव तब उत्पन्न होता है, जब अहंकार और मन विलीन हो जाते हैं। यह व्यक्ति के स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त होती है। यह असीम, अविभाज्य तथा अनन्त अस्तित्व तथा शुद्ध चेतना का अनुभव है। जब इस अनुभव का साक्षात्कार होता है, तो खुशी तथा दुःख की भावना तथा मन, कामनाएँ एवं कर्म नष्ट हो जाते हैं।
अन्तिम सत्य अथवा ब्रह्म अथवा परमात्मा का अनुभव सभी लोगों के द्वारा शुद्ध हृदय सहित ध्यान के नियमित अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। मात्र निर्गुण चिन्तन एवं पुस्तकों के अध्ययन से ऐसा सम्भव नहीं है। जो चाहिए, वह है प्रत्यक्ष अनुभवा प्रत्यक्ष अनुभव उच्च अन्तर्ज्ञान अथवा दैवी प्रज्ञा का स्रोत है। यह अनुभव परम चेतना है। वहाँ न तो इन्द्रियों का खेल है, न ही वहाँ बुद्धि है। यह एक आवेगात्मक अनुभव नहीं है। इन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि पूर्ण विश्राम में रहती हैं। वे थोड़ा भी कार्य नहीं करतीं। यह स्वप्न देखने वाले के अनुभवों की भाँति एक काल्पनिक अनुभव नहीं है। यह दिवा स्वप्न नहीं है। यह आपकी हथेली पर आँवले के फल की भाँति ठोस जीवित सत्य है। अनुभवकर्ता में तृतीय नेत्र अथवा ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। अतिविशिष्ट अनुभव आध्यात्मिक नेत्रों अथवा ज्ञान चक्षु से बोध प्राप्त करने से आता है। ज्ञान चक्षु तभी खुल सकते हैं, जब इन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि कार्य करना बन्द कर देते हैं। तृतीय नेत्र अथवा ज्ञान चक्षु सभी कामनाओं, क्रोध, लोभ, अहंकार, स्वार्थ तथा घृणा के पूर्ण उन्मूलन करने पर खुल, सकते हैं।
इस अनुभव में न अन्धकार है, न शून्य ही है। यह पूर्ण प्रकाशमय है। वहाँ न ध्वनि, न स्पर्श, न रूप है। यह एकता का महान् अनुभव है। यहाँ न समय, न सावधानी है। आप सर्वव्यापक, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। आप सर्वविद् अथवा सर्वज्ञाता बन जाते हैं। आप प्रत्येक वस्तु को विस्तृत रूप में जानते हैं। आप सृष्टि का सम्पूर्ण रहस्य जानते हैं। आप अमरता, उच्च ज्ञान तथा परमानन्द प्राप्त करते हैं।
सभी द्वैतभाव यहाँ नष्ट हो जाते हैं। वहाँ न विषय, न पात्र ही है। वहाँ न साकार है न निराकार। न वहाँ ध्यान है न समाधि। वहाँ न द्वैत है न अद्वैत वहाँ न ध्याता है न ध्येया वहाँ न लाभ है न हानि। वहाँ न सुख है न दुःखा वहाँ न पूरब है न पश्चिम। न यहाँ दिन है न रात्रि।
समाधि अनेक प्रकार की है। वह समाधि जो मुद्रा तथा प्राणायाम के अभ्यास से प्रेरित होती है, वह जड़ समाधि है। वहाँ कोई चैतन्यता नहीं होती। एक योगी को पृथ्वी के नीचे एक डिब्बे में बन्द करके ६ माह के लिए गाड़ दिया जा सकता है। यह गहन निद्रा की भाँति है। योगी इससे आध्यात्मिक ज्ञान के साथ वापस नहीं आता। इस समाधि से वासनाएँ नष्ट नहीं की जा सकती। योगी पुनः जन्म लेगा। इस समाधि से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इसके बाद है चैतन्य समाधि। इसमें योगी को पूर्ण चैतन्यता रहती है। वह देवी ज्ञान के साथ वापस आता है। वह प्रेरणाप्रद प्रवचन और सन्देश देता है, जिनको सुनने से सुनने वालों का अत्यधिक उत्थान होता है। वासनाएँ इस समाधि से नष्ट हो जाती हैं। योगी को कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है।
एक भक्त द्वारा जिस समाधि का अनुभव किया जाता है, वह भाव समाधि है। भक्त यह अवस्था भाव तथा महाभाव से प्राप्त करता है। राजयोगी निरुद्ध समाधि संकल्पों (चित्तवृत्तिनिरोध) के नाश के द्वारा प्राप्त करता है। वेदान्ती भ्रामक साधनों अथवा उपाधियों जैसे मन, शरीर, इन्द्रियों, बुद्धि आदि के निरोध के द्वारा समाधि प्राप्त करता है। उसके लिए जगत् एवं शरीर अवास्तविक अथवा मिथ्या है। वह अन्धकार, प्रकाश, निद्रा, मोह तथा अनन्त आकाश की अवस्थाओं से गुजरता है और अनन्त चेतना प्राप्त करता है।
इसके बाद पुनः समाधि के दो अन्य प्रकार हैं सविकल्प अथवा सबीज या सम्प्रज्ञात समाधि एवं निर्विकल्प अथवा निर्बीज अथवा असम्प्रज्ञात समाधि प्रथम प्रकार में त्रिपुटी अर्थात् ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय अथवा द्रष्टा, दृश्य और दृष्टव्य का समूह होता है। इसके संस्कार नष्ट नहीं होते। बाद वाली में संस्कार पूर्ण दग्ध अथवा नष्ट हो जाते हैं। निर्विकल्प में कोई त्रिपुटी नहीं है। सविकल्प, निर्विचार, सदानन्द-ये सविकल्प समाधि के प्रकार हैं।
जब आप उच्च निर्विकल्प समाधि में होते हैं, तो आपको कोई चीज नहीं दिखायी देती, कुछ सुनायी नहीं देता, किसी प्रकार की गन्ध नहीं आती, किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता। आपको किसी प्रकार की शारीरिक चेतना नहीं होती। आपको पूर्ण ब्रह्म चेतना रहती है। वहाँ और कुछ नहीं है, मात्र आत्मा है। यह एक बड़ा अनुभव है। आप आश्चर्य से भौंचक्के रह जायेंगे।
एक भक्त जो कि भगवान् कृष्ण के रूप पर ध्यान करता है, जब वह समाधि में स्थापित हो जायेगा, तो वह सर्वत्र मात्र कृष्ण को ही देखेगा। सभी अन्य रूप नष्ट हो गये हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव है। वह स्वयं को कृष्ण की तरह देखेगा। वृन्दावन की गोपियों, गौरांग तथा एकनाथ को इस प्रकार का अनुभव था। जो सर्वव्यापक कृष्ण पर ध्यान करते हैं, उन्हें एक भिन्न प्रकार की दैवी चेतना होती है। अर्जुन को इस प्रकार का अनुभव था। उसे सम्पूर्ण विराट् की चेतना थी। उसे ब्रह्माण्डीय देवी चेतना थी।
यदि आप हिरण्यगर्भ पर ध्यान करेंगे, तो आप हिरण्यगर्भ के साथ एक बन "जायेंगे। आपको ब्रह्मलोक का ज्ञान होगा। आपको दैवी चेतना भी होगी। एक भक्त और राजयोगी को सविकल्प समाधि का अनुभव एक जैसा होता है।
सर्वोच्च अनुभव को भी तुरीयावस्था अथवा चतुर्थ अवस्था कहते हैं। प्रथम तीन अवस्थाएँ हैं जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था और चौथी है तुरीयावस्था। प्रथम तीन अवस्थाएँ सभी में एक समान हैं तथा चतुर्थ प्रत्येक मनुष्य में छुपी है। जब आप चतुर्थ अवस्था में स्थापित हो जायेंगे, जब आप ब्रह्मचेतनावस्था की सर्वोच्च अवस्था, वह सत्य जो कि पहले है, लेकिन एक बौद्धिक कल्पना की भाँति एक जीवित सत्यता निश्चित रूप से आपके द्वारा अनुभव की जाती है।
अनेक नाम जैसे सम्यक् दर्शन, सहज अवस्था, निर्वाण, तुरीयातीत, अपरोक्ष भावना, ब्रह्म-साक्षात्कार, निर्विकल्प समाधि, असम्प्रज्ञात अवस्था इस अवस्था को दिये गये हैं, लेकिन सभी एक ही लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं। सच्चा आध्यात्मिक जीवन जब कोई इस परम चेतनावस्था में प्रवेश करता है, तब प्रारम्भ होता है।
आप सारे समय एवं सभी अवस्थाओं में साक्षात्कार करें कि आप अदृश्य अस्तित्व ज्ञान तथा आनन्द के साथ एक हैं, आपने सभी व्यक्तियों और विषयों को व्याप्त कर रखा है तथा आप सभी सीमाओं से परे हैं। यदि आपको सारे समय बिना किसी आत्मा अथवा ब्रह्म का ज्ञान है, तब आप आत्मा में स्थापित हैं। यह वह अवस्था है जिसका भीतर में अनुभव किया जा सकता है, किन्तु इसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यह शान्ति की अन्तिम अवस्था तथा जीवन का लक्ष्य है। यह अनुभव सभी प्रकार के बन्धनों से आपको मुक्ति देगा।
कुछ साधक गहन निद्रावस्था तथा तन्द्रा अथवा अर्धनिद्रावस्था को निर्विकल्प समाधि समझ लेते हैं। यह एक भयंकर भूल है। यदि आप किसी भी प्रकार की समाधि का अनुभव करेंगे, तो आपको परम ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आपको किसी प्रकार का अन्तर्ज्ञान नहीं हो, तो निश्चय मानें कि आप समाधि से दूर हैं। आप समाधि का अनुभव मात्र करेंगे, जब आप यम, नियम, सदाचार में स्थापित होंगे तथा जब आपका हृदय स्थिर होगा। अस्थिर हृदय में भगवान् कैसे सिहासनारूढ़ हो सकते हैं। समाधि मात्र निरन्तर तथा संरक्षित ध्यान के अभ्यास से ही आती है। समाधि वह वस्तु नहीं है जो सरलता से प्राप्त हो सके। जो समाधि में वास्तव में प्रवेश करते हैं, वे लोग अत्यन्त दुर्लभ हैं।
समाधि अथवा परम चेतनावस्था में योगाभ्यासी स्वयं को भगवान में लीन पाता है। इन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि कार्य करना बन्द कर देते हैं। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। सभी सीमाएँ तथा भेद अदृश्य हो जाते हैं। योगी परम ज्ञान तथा परमानन्द प्राप्त करता है। यह स्थिति वर्णन से परे है। आपको इसका साक्षात्कार स्वयं करना होगा।
अपने भीतर की आत्मा में सुन्दर जीवन की अमर मिठास का स्वाद लीजिए। आत्मा में निवास कीजिए तथा अमर अवस्था को प्राप्त कीजिए। ध्यान करें तथा अनन्त जीवन की गहन गहराइयों में तथा दैवी वैभव की ऊँचाइयों को प्राप्त करें। अब आपकी लम्बी अथक यात्रा समाप्त हो गयी है। आप अपने गन्तव्य, अपने स्थायी शान्ति के वास्तविक घर, परम धाम पहुँच गये हैं।
१०. मन भ्रमण करता है
ध्यान के थोड़े अभ्यास के बाद आप अनुभव करेंगे कि शरीर थोड़े समय में ही अर्थात् जब आप पद्म, सिद्ध अथवा सुखासन में बैठते हैं (अपनी रुचि या स्वभाव के अनुसार), उसके १५ या १० मिनट बाद आप शरीर को हल्का अनुभव करते हैं।
आप शरीर की अर्धचेतनावस्था में भी हो सकते हैं। धारणा के कारण आपको बहुत आनन्द का अनुभव होगा। यह प्रसन्नता धारणा के आनन्द का परिणाम है, जो कि इन्द्रिय-सुखों से बिलकुल भिन्न है। आपको इन दोनों सुखों में भिन्नता करने में उस बुद्धि के द्वारा सक्षम होना चाहिए, जो निरन्तर अभ्यास, ध्यान, धारणा तथा ध्यान के द्वारा सूक्ष्म हो गयी है। धारणा तथा ध्यान में बुद्धि को तीक्ष्ण करने की शक्ति है। प्रशिक्षित बुद्धि सूक्ष्म दार्शनिक समस्याओं को सुन्दर तरीके से समझ सकती है। संयमित बुद्धि जो सावधानीपूर्वक धारणा के आनन्द तथा निदिध्यासन के आनन्द में विभेद कर सकती है, वह स्वाभाविक रूप से नित्य इस नये आनन्द की ओर भागेगी। ऐसा मन विषय सुखो को नापसन्द करेगा। वहाँ विषयों के प्रति सकारात्मक तथा अत्यधिक घृणा होगी। यह प्राकृतिक होगा, क्योंकि इस प्रकार का आनन्द अधिक स्थायी, स्थिर, आत्म सन्तुष्ट तथा वास्तविक होगा, क्योंकि यह आत्मा से निकलता है। आप स्पष्टतया अनुभव करेंगे कि मन घूम रहा है, यह मस्तिष्क के अपने स्थान को छोड़ रहा है तथा यह इसके यथास्थान को जाने का प्रयास कर रहा है। आप जानते हैं कि इसने अपनी पुरानी खाई को छोड़ दिया है तथा अब यह अपनी लीकों में नयी खाई में जा रहा है। ध्यान के परिणामस्वरूप मस्तिष्क में नयी लीक बनती है तथा नयी विचार तरंगें बनती है तथा नवीन मस्तिष्क कोशिकाएँ बनती हैं। वहाँ इसके साथ ही रूपान्तरित मनोवैज्ञानिकता है। आपने एक नया मस्तिष्क, नवीन हृदय, नयी भावनाएँ, नयी संवेदनाएँ प्राप्त की हैं।
११. भूत गण
ये भूत गण कभी-कभी ध्यानावस्था में गोचर होते है। इनका रूप विचित्र होता है— किसी के दाँत लम्बे, किसी कर चेहरा बड़ा, किसी का पेट मोटा, किसी के पेट पर चेहरा, किसी के सिर पर मुखा ये सब भूलोक के निवासी है। ये भूत हैं। ये सब भगवान् शिव के अनुचर माने जाते हैं। इनका रूप भयानक होता है। ये बिलकुल निरापद है। ये रंगमंच पर केवल दिखायी देते हैं। ये आपकी शक्ति और साहस परखने आते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नीतिवान्, चरित्रवान् साधक के सामने ये खड़े भी नहीं रह सकते। ॐ का जप उन्हें फेंक देता है। आपको निर्भय रहना चाहिए। भीरु व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। सदा इस अनुभूति के द्वारा कि आप आत्मा हैं, साहस का विकास कीजिए। देहभाव को अस्वीकार कीजिए। चौबीसों घण्टे निदिध्यासन कीजिए। यह रहस्य है। यही कुंजी है। यह सच्चिदान्द-रूपी कोष के द्वार को खोलने की कुंजी है। आनन्द रूपी भवन की यह आधारशिला है। आनन्द के राजप्रासाद का यह प्रमुख स्तम्भ है।
१२. आत्मा की झलक
अच्छे तथा बुरे अनुभवों से मनुष्य पदार्थों को एकत्र करता है तथा उनको मानसिक तथा नैतिक योग्यताओं में निर्मित करता है। जिस प्रकार एक व्यापारी वार्षिक बही-खाते को बन्द करता है तथा नयी बही खोलने के बाद इसमें पुरानी सभी चीजें नहीं लिखता, वह मात्र इसमें उनका जोड़ ही लिखता है। इसी प्रकार आत्मा नये मस्तिष्क को बीते जीवन के अनुभवों और निर्णयों तथा हलों को स्थानान्तरित कर देता है। यह सामान, मानसिक फर्नीचर नवीन जीवन तथा नवीन निवासी को दे दिया जाता है, जो कि सच्ची स्मृति है।
मन जो कामनाओं के पतन से सदा उठता और गिरता है, इस भ्रामक विश्व को यह अपनी अज्ञानता के कारण सत्य कल्पना करता है। लेकिन इसे जगत् की वास्तविक प्रकृति बतायी जानी चाहिए। तब इसे स्वयं ब्रह्म बनने का ज्ञान होगा।
ध्यान के समय आप अनुभव करेंगे कि आप अपने स्थान से ऊपर उठ रहे हैं। कुछ को ऐसा अनुभव होता है कि वे हवा में उड़ रहे हैं।
अनेक लोग अनेक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। वहाँ सभी के लिए एक जैसा अनुभव नहीं हो सकता। यह स्वभाव साधना की विधि, धारणा का स्थान तथा अन्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। कुछ कानों में मधुर ध्वनियाँ सुनते हैं। कुछ प्रकाश देखते हैं। कुछ आनन्द (आध्यात्मिक आनन्द) प्राप्त करते हैं। कुछ दोनों ही प्राप्त करते हैं- प्रकाश एवं आनन्द
यदि साधना में कोई गलती है, तो तत्काल वरिष्ठ संन्यासियों अथवा साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं से सलाह लें और गलती को दूर करिए। यदि आपका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा है, यदि आप उत्साहित, प्रसन्न हैं तथा शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ हैं, यदि मन शान्तिपूर्ण है तथा अविचल है, यदि आप ध्यान में आनन्द प्राप्त करते हैं तथा यदि आपका संकल्प दृढ़, शुद्ध तथा अटल है, तो आप सोचें कि आप ध्यान में विकास कर रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा है।
दैवी प्रकाश खुले द्वार से नहीं आता, बल्कि सँकरी गलियों से आता है। साधक एक किरण देखता है, जिस प्रकार सूर्य की किरण एक अँधेरे कमरे में एक चिक से आती । यह एक बिजली की चमक की भाँति है। यह अचानक आने वाला प्रकाश शब्दों की सभी ध्वनियों को रोक देता है। साधक भावोत्कर्ष एवं भय में मूक हो जाता है। वह प्रेम तथा भय से काँपने लगता है जैसा कि भगवान् कृष्ण के विराट् स्वरूप के दर्शन से अर्जुन ने किया था। दैवी के चारों ओर का प्रकाश इतना चमकदार तथा सुन्दर होता है कि शिष्य चकरा जाता है और भ्रमित हो जाता है।
यह दृश्य व्यक्ति ध्यान के समय कभी-कभी प्राप्त करता है। आप अचानक तीव्र गति से चमकदार प्रकाश देख सकते हैं। आप एक सिर को देखते हैं अद्भुत रूपों वाला, ज्योति के रंग का, अग्नि की भाँति लाल तथा जो देखने में अत्यन्त भयंकर होता है। इसके तीन पंख होते हैं, इसकी लम्बाई तथा चौड़ाई अद्भुत होती है और यह बादल की तरह सफेद होते हैं। कभी-कभी वे बुरी तरह फड़फड़ायेंगे और बाद में स्थिर हो जायेंगे। सिर कभी भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। लेकिन साथ-साथ स्थिर रहेगा। अब पुनः इसके लम्बे पंखों के साथ फड़फड़ाहट होगी।
ध्यान के समय प्रकाशों के रंग जो आप देखते हैं, वे उस तत्त्व की प्रकृति के अनुसार होते हैं जो उस समय नासारन्ध्रों से प्रवाहित होता है। यदि वहाँ अग्नि तत्त्व प्रवाहित होगा, तो आप लाल रंग का प्रकाश देखेंगे। यदि आकाश तत्त्व प्रवाहित होगा, तो आप नीले रंग का प्रकाश देखेंगे। यदि जल तत्त्व प्रवाहित होगा, तो आप श्वेत रंग का प्रकाश देखेंगे। यदि वायु तत्त्व प्रवाहित होगा, तो आप काले रंग का प्रकाश देखेंगे। आप अनेक प्रकार से तत्त्व-परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है विचार द्वारा जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। जब अग्नि तत्त्व प्रवाहित हो, तो प्रबलता से जल तत्त्व के बारे में सोचें। शीघ्र ही आप में वह तत्त्व प्रवाहित होने लगेगा।
यदि आप प्रबल ध्यान के समय आत्मा की झलक का अनुभव करें, यदि आप ध्यान के समय चमकदार प्रकाश देखें तथा यदि आप देवदूतों, ऋषियों-मुनियों और देवताओं के आध्यात्मिक दर्शन तथा अन्य कोई अतिविशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव करें, तो भयभीत हो कर वापस न लौटें। उन्हें भूत न समझें। साधना न छोड़ें। सावधानी के साथ आगे बढ़ें। आवरण के बाद आवरण तोड़ते जायें।
साहस के साथ आगे बढ़ें। पीछे न देखें। प्रबल शून्य तथा अन्धकार को पार करें। मोह की पर्त को भेदें। सूक्ष्म अहंकार को अब पिघला दें। स्वरूप स्वयं ही प्रकाशित होगा। आप तुरीयावस्था (अरुद्ध अवस्था) का अनुभव करेंगे।
कभी-कभी बुरी आत्माएँ आपको परेशान करेंगी। उनके भयंकर चेहरे लम्बे दाँतों के साथ हो सकते हैं। उन्हें अपने दृढ़ संकल्प से भगा दें। आदेश दें – “बाहर जाओ।" वे चली जायेंगी। वे पिशाच हैं। वे प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। वे साधकों को कोई हानि नहीं पहुँचायेंगी। वहाँ आपके साहस की परीक्षा ली जा रही है। यदि आप डरपोक हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पायेंगे। अपने भीतर आत्मा के अक्षय स्रोत से साहस और शक्ति खींचें। आपके पास कुछ अत्यधिक अच्छी आत्माएँ भी आयेंगी। वे आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। ये सभी मार्ग में विघ्न हैं।
साधक आध्यात्मिक अनुभव शीघ्र प्राप्त करने हेतु उत्सुक रहते हैं। जैसे ही वे उन्हें प्राप्त करते हैं, वे घबरा जाते हैं। जब वे शरीर-चेतना से ऊपर उठ जाते हैं, तो वे भयंकर रूप से घबरा जाते हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि वे वापस आ सकेंगे या नहीं। वे डरते क्यों हैं? इसमें क्या है वे वापस आ सकेंगे या नहीं। हमारे सभी प्रयत्न मुख्य रूप से शरीर चेतना से ऊपर उठने तथा उच्च आध्यात्मिक चेतना से एक होने के लिए हैं। हम कुछ सीमाओं के आदी हैं। जब वे सीमाएँ अचानक टूट जाती हैं, तो हमें अनुभव होता है कि खड़े रहने के लिए हमारे पास निश्चित आधार ही नहीं है। यही वह कारण है कि जब हम शरीर की चेतना से ऊपर जाते हैं, तो हमें डर का अनुभव होता है। यह एक अपूर्व अनुभव है। साहस की आवश्यकता है। साहस एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। श्रुति कहती है — “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।” यह आत्मा दुर्बल लोगों को प्राप्त नहीं होती। मार्ग में सभी प्रकार की शक्तियों से संघर्ष होता है। एक डकैत अथवा एक अराजकतावादी भगवान् का साक्षात्कार सरलता से कर सकता है; क्योंकि वह निर्भय है। सही दिशा में एक धक्के की ही मात्र उसके लिए आवश्यकता है। जगाई और मधाई प्रथम श्रेणी के डकैत, बहुत अच्छे सन्त किस प्रकार बने? उन्होंने भगवान् गौरांग के शिष्य नित्यानन्द पर पत्थर फेंके। नित्यानन्द ने उन्हें पवित्र दैवी प्रेम से जीता। डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बने।
१३. ज्योतिर्मय दर्शन
जब आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने इष्टदेवता को शारीरिक रूप में देखेंगे। भगवान् विष्णु आपको चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे। भगवान् श्री कृष्ण आपके सामने मुरली लिये हुए प्रकट होंगे। राम धनुष-बाण अपने हाथ में लिये आपके सामने प्रकट होंगे।
कभी-कभी भगवान् आपके सामने भिखारी अथवा रोगी व्यक्ति के रूप में फटे कपड़ों में प्रकट होंगे। वे आपके सामने कुली अथवा शूद्र के रूप में प्रकट हो सकते हैं। आपको उनको पहचानने की सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। आप जब उनसे मिलेंगे, तो आपके रोंयें खड़े हो जायेंगे।
वे आपके स्वप्न में प्रकट होंगे। भगवान् गणेश स्वप्न में हाथी के रूप में आते हैं। देवी स्वप्न में लड़की के रूप में आती हैं।
गहन ध्यान में आपको ज्योति के दर्शन होंगे। आप एक प्रकाश का बड़ा स्तम्भ देखेंगे। आप अनन्त प्रकाश देखेंगे और स्वयं को इसमें लीन कर देंगे। आप भय तथा आश्चर्य से भौंचक्के रह जायेंगे।
यदि आप तीव्रता से निरन्तर भगवान् श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आप सर्वत्र भगवान् श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे।
एक योगी को भय, क्रोध, आलस्य, अत्यधिक निद्रा अथवा जागरण तथा भोजन एवं उपवास की उपेक्षा करनी चाहिए। यदि उपर्युक्त नियम का भली प्रकार एवं कठोरता से प्रति दिन अभ्यास किया जाये, तो आध्यात्मिक ज्ञान निःसन्देह तीन माह के भीतर स्वयं ही जागेगा। चार माह में वह देवताओं के दर्शन करेगा। उसे पाँच माह में उसे ब्रह्मनिष्ठा का ज्ञान होगा (अथवा वह ब्रह्मनिष्ठ बन जायेगा) तथा छह माह के भीतर संकल्प से कैवल्य प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है।
परिशिष्ट
एकाग्रता का परीक्षण
दक्षिण भारत के एक तमिल सन्त तिरुवल्लुवर ने अपनी पत्नी के सिर पर जल से भरी एक थाली रख दी और आदेश दिया कि गाँव-भर में उसे सिर पर रख कर घूम कर आओ, जल की एक बूँद भी यदि भूमि पर गिरी तो सिर काट दिया जायेगा। त्रिचिनापल्ली के निकट श्रीरंगम् के विशाल मन्दिर के प्रमुख द्वार से जुलूस निकला। तिरुवल्लुवर की पत्नी जल से भरी उस थाली को अपने सिर पर रखे जुलूस के साथ चली। उसका सारा प्राण, सारा मन और सम्पूर्ण हृदय जल की उस थाली में केन्द्रित था। वह जुलूस नगर के चार मार्गों में तीन बार घूमने के पश्चात् जहाँ से आरम्भ हुआ था वहीं मन्दिर के द्वार पर आ कर समाप्त हुआ। सन्त की पत्नी जल की एक बूँद भी भूमि पर गिराये बिना वापस आ गयी। तिरुवल्लुवर ने अपनी पत्नी से पूछा- “हे सरस्वती, क्या तुमने जुलूस के साथ बजने वाले संगीत तथा वंशी को सुना और नृत्य को देखा?” उसने कहा—“नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना और न मैं कुछ जान सकी। मुझे कुछ स्मरण नहीं आया और न मैंने कुछ देखा ही। मेरा सम्पूर्ण मन तो जल की थाली में था।'
अब यहाँ देखें। सन्त की पत्नी का मन पूर्ण एकाग्र था। अतः उसने न कुछ सुना, न देखा, न अनुभव किया और न कुछ स्मरण किया। ध्यानावस्था में आपके मन की स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए। इसी का नाम एकाग्रता है। अखण्ड अवधान, अखण्ड शक्ति होनी चाहिए। ईश्वर की ओर सारा ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। तभी आप ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। तभी आप जीवन की कठिन समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।
द्रोण तथा उनके शिष्य
द्रोणाचार्य तथा उनके शिष्यों के मध्य की निम्न वर्णित वार्ता आपके लिए बहुत ही रुचिकर होगी।
द्रोण: युधिष्ठिर, तुम क्या देख रहे हो?
युधिष्ठिर: आचार्य जी, मैं अपने लक्ष्य उस पक्षी को तथा जिस वृक्ष पर वह बैठा है उस वृक्ष को और अपने बगल खड़े आपको देख रहा हूँ।
द्रोण: तुम्हें क्या दिख रहा है भीम?
भीम : मुझे वह पक्षी, वृक्ष, आप, नकुल, सहदेव तथा भूमि पर खड़े वृक्ष तथा पौधे दिख रहे हैं।
द्रोण: नकुल, तुम्हें क्या दिखता है?
नकुल : मुझे पक्षी, वृक्ष, अर्जुन, भीम, उपवन, सरिताएँ आदि दिखायी दे रही हैं।
द्रोण: तुम क्या देखते हो सहदेव ?
सहदेव : मैं लक्ष्य, पक्षी, वृक्ष, आप, भीम, युधिष्ठिर, घोड़े, रथ, ये सब दर्शक, अनेक गायों आदि को देख रहा हूँ।
द्रोण: क्यों अर्जुन, तुम्हें क्या दिखता है?
अर्जुन : पूज्य गुरु जी ! अपने लक्ष्य उस पक्षी के अतिरिक्त मुझे अन्य कुछ भी नहीं दिख रहा है।
उपर्युक्त पाठ से यह स्पष्ट है कि जब आपका मन किसी विशेष पदार्थ पर एकाग्र हो जाता है, तब आप अन्य कुछ भी देख अथवा सुन नहीं सकते। आपमें उपासना तथा योग के द्वारा मन के विक्षेप के निवारण से ध्यान के लिए अर्जुन के समान ही एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता के विकास के लिए त्राटक तथा प्राणायाम भी सहायक होते हैं। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि एकमात्र अर्जुन में ही गम्भीर एकाग्रता थी।
शुकदेव
महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव अपने कुछ विशेष दार्शनिक प्रश्नों के लिए अपने पिता द्वारा दिये गये उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं थे। अतः श्री व्यास जी ने उन्हें मिथिलानरेश के पास भेजा।
शुकदेव राजा जनक के महल के द्वार पर तीन दिनों तक भूखे-प्यासे प्रतीक्षा करते रहे। जनक शुकदेव की परीक्षा लेना चाहते थे कि वे सन्तुलित मन तथा समदृष्टि वाले हैं या नहीं। तीन दिनों पश्चात् शुकदेव को महल में ले जाया गया और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन दिये गये और उनका बड़ा ही आदर-सत्कार किया गया। कई महिलाएँ उनकी सेवा कर रही थीं। शुकदेव उन्हें दरवाजे के बाहर बिना भोजन के रखने से न तो हताश हुए, न ही महल में शाही व्यवहार से प्रसन्न हुए। उनका दोनों विभिन्न अवसरों पर वही सन्तुलित मन रहा।
जनक शुकदेव की एकाग्र शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। उन्होंने उनको एक प्याला दिया जो तेल से लबालब भरा हुआ था और उनसे कहा गया कि वे प्याले को हाथ में ले कर पूरी मिथिला नगरी का चक्कर लगा कर आयें और इसमें से एक बूँद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। जनक ने शहर के चारों ओर नृत्य-संगीत की सभाओं का आयोजन किया था।
शुकदेव ने प्याला हाथ में लिया और तेल की एक भी बूँद भूमि पर गिराये बिना प्याले को वापस ले कर आये, क्योंकि उनमें प्रबल धारणा तथा इन्द्रिय-संयम था। वे बाह्य ध्वनियों तथा वस्तुओं से तनिक भी आकृष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे प्रत्याहार में भलीभाँति स्थापित थे। उनका मन तेल के कप पर सदा एकाग्र था।
आपकी भी धारणा-शक्तिशुकदेव की भाँति होनी चाहिए।
तीर बनाने वाला
एक तीर बनाने वाला अपने कार्य में व्यस्त था। वह अपने कार्य में पूर्णतया तल्लीन था। उसकी धारणा प्रबल थी। एक बार राजा और उसकी सवारी उसकी कार्यशाला के सामने से निकली। चूँकि वह अपने कार्य में पूरी तरह तल्लीन था, इस कारण उसे उन सबका पता ही नहीं चला। आपकी भी धारणा-शक्ति उस तीर बनाने वाले के समान ही होनी चाहिए।
भगवान् दत्तात्रेय ने इसी तीर बनाने वाले से मन की एकाग्रता सीखी। उन्होंने इसे अपना एक गुरु माना था। श्वास पर नियन्त्रण प्राप्त करके तथा आसन में स्थिरता प्राप्त करके, आप उस तीर बनाने वाले की तरह अपना लक्ष्य ले कर मन को परमात्मा पर केन्द्रित करें। मन को ध्यान के विषय में पूर्णतया लीन होना चाहिए। अपने मन को आत्मा में पूर्णतः लीन करके आपको उस समय भीतर अथवा बाहर किसी भी विषय को नहीं देखना चाहिए जिस प्रकार उस तीर बनाने वाले ने पास से जा रही राजा की सवारी को नहीं देखा था।
नेपोलियन बोनापार्ट
नेपोलियन बोनापार्ट की धारणा अद्भुत थी। उसकी सफलता मात्र उसकी धारणा के ही कारण थी। उसे अनेक प्रकार के गम्भीर रोग थे, किन्तु उन रोगों के लिए वह बहुत शक्तिशाली और आश्चर्यजनक सिद्ध हुई। वह जिस समय चाहता, उस समय सो सकता था और वह बिस्तर में लेटते ही गहरी निद्रा में चला जाता था। वह जिस समय चाहे, उसी क्षण जाग सकता था। यह एक प्रकार की सिद्धि होती है ।
उसके मस्तिष्क में डाकघर के पत्र रखने के अनेक खानों की तरह अनेक कोष्ठक थे। उसके भीतर किसी प्रकार के विक्षेप नहीं थे। उसके पास एक योगी का अत्यधिक विकसित एकाग्र चित्त था। वह अपने मस्तिष्क के कोष्ठक से कोई विचार निकाल कर जब तक उस पर चाहता, विचार करता और जब चिन्तन समाप्त हो जाता, तो उसे वापस भेज सकता था। वह युद्ध के बीच रात्रि के समय गहरी नींद सो सकता था और इस समय उसे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती थी। यह सब मात्र धारणा-शक्तिके कारण ही था। उसने यह सिद्धि त्राटक के अभ्यास से नहीं प्राप्त की थी, वरन् एक अर्थ में वह योगभ्रष्ट (योगभ्रष्ट अर्थात् जो पूर्व जन्म में योग-मार्ग से च्युत हो गया हो) और जन्म से सिद्ध था।
संयोजन का नियम
जब आप सन्ध्या के समय लारेंस गार्डन में भ्रमण हेतु जाते हैं, तो आपको कालेज के दो लड़के हेनरी और थॉमस मिलते हैं। एक दिन आप हेनरी को अकेले देखते हैं, तो सोचते हैं थामस नहीं आया। जब भी आप हेनरी को देखते हैं, तो थामस का विचार आपके मन में संयोजन के नियम के कारण आता है।
जब आप गंगा नदी के बारे में विचार करते हैं, तो आप यमुना और गोदावरी के बारे में भी विचार कर सकते हैं। जब आप गुलाब के बारे में विचार करते हैं, तो आप चमेली के बारे में विचार कर सकते हैं। जब आप सेबफल के बारे में विचार करते हैं, तो आप आम के बारे में भी विचार कर सकते हैं। यह संयोजन का नियम है।
आप विचारों तथा वस्तुओं के संयोजन के द्वारा अपनी स्मृति का विकास कर "सकते हैं। हिन्दी में पाव का अर्थ है चौथाई। पाव का प्रतिबिम्ब मन में रखिए। आप नवधा भक्ति के दो अंगों जैसे पाद सेवन और वन्दना जो कि पा और व से प्रारम्भ होते है, को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार आप शब्दों तथा अक्षरों के प्रतिबिम्ब से अपने मन के विभिन्न विचारों को जोड़ सकते हैं। जिन्होंने इस आदत को इस जन्म में अर्जित किया है, वे बड़ी ही उत्तम और दृढ़ स्मृति से सम्पन्न होते हैं।
यदि आप मन के भटकाव को ध्यान से देखेंगे, आप पायेंगे कि वहाँ एक विचार का दूसरे विचार के मध्य बड़ा ही अन्तरंग सम्बन्ध है, जिनके द्वारा यह मन एक बिना जंजीर से बँधे बन्दर की भाँति इधर से उधर भटकता रहता है। कड़ी टूट भी जायें, तो भी संयोजन का नियम कार्य करता है। मन एक पुस्तक के बारे में विचार करता है, उसके बाद उस दूकान के बारे में जहाँ से श्रीमान् जान ने इसे खरीदा था। उसके बाद उस मित्र के बारे में जिससे रेलवे स्टेशन पर तब मिले थे जब यह पुस्तक खरीदी गयी थी, उसके बाद रेलवे तथा रेलवे के निर्देशक के बारे में जो लन्दन में रहते हैं। लन्दन का विचार शायद स्केटिंग के विचार को लाये, स्केटिंग के विचार से यह एल्पस को कूद जाये। यह चीड़ के वृक्षों, सेनिटोरियम तथा खुली वायु में उपचार के बारे में विचार कर सकता है। चीड़ के वृक्ष का विचार भारत के अल्मोड़ा तथा इसके पास जहाँ चीड़ के वृक्ष उत्पन्न होते हैं, का स्मरण करायेगा। अल्मोड़ा का विचार स्वामी विवेकानन्द का स्मरण करायेगा, जिन्होंने अल्मोड़ा के पास मायावती में अद्वैत आश्रम स्थापित किया। यह धारणा और ध्यान तथा अद्वैत ब्रह्म के कुछ दैवी विचारों पर चिन्तन कर सकता है। तब अचानक यह विषयी गलियों में चला जायेगा। यह अल्मोड़ा की वेश्याओं के बारे में विचार कर सकता है। यह वासनात्मक विचार करने लगेगा।
ये सब पलक झपकते ही हो जायेगा। मन आश्चर्यजनक गति से कार्य करता है, जिसका अनुमान लगाना कठिन है। यह एक विषय को पकड़ता है और संयोजन के द्वारा एक विचार का निर्माण करता है। यह इस विषय और धारणा को छोड़ कर अन्य विषय और विचार पर कूद जाता है। यह इसके समस्त भ्रमण में एक प्रकार की धारणा है, हालाँकि यह धारणा निरन्तर नहीं है।
हरि ॐ तत्सत्!
बीस महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक नियम
(परम श्रद्धेय श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज)
१. ब्राह्ममुहूर्त-जागरण— नित्यप्रति प्रातः चार बजे उठिए। यह ब्राह्ममुहूर्त ईश्वर के ध्यान के लिए बहुत
अनुकूल है।
२. आसन — पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन पर जप तथा ध्यान के लिए आये घण्टे के लिए पूर्व
अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। ध्यान के समय को शनैः-शनैः तीन घण्टे तक बढ़ाइए। ब्रह्मचर्य तथा स्वास्थ्य के लिए शीर्षासन: अथवा सर्वांगासन कीजिए। हलके शारीरिक व्यायाम (जैसे टहलना आदि) नियमित रूप से कीजिए। बीस बार प्राणायाम कीजिए।
३. जप – अपनी रुचि या प्रकृति के अनुसार किसी भी मन्त्र (जैसे 'ॐ', 'ॐ नमो नारायणाय', 'ॐ नमः
शिवाय', 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय', 'ॐ श्री शरवणभवाय नमः', 'सीताराम', 'श्री राम', 'हरि ॐ' या गायत्री) का १०८ से २१,६०० बार प्रतिदिन जप कीजिए (मालाओं की संख्या १ और २०० के बीच) ।
४. आहार - संयम — शुद्ध सात्त्विक आहार लीजिए। मिर्च, इमली, लहसुन, प्याज, खट्टे पदार्थ, तेल,
सरसों तथा हींग का त्याग कीजिए। मिताहार कीजिए। आवश्यकता से अधिक खा कर पेट पर बोझ न डालिए। वर्ष में एक या दो बार एक पखवाड़े के लिए उस वस्तु का परित्याग कीजिए जिसे मन सबसे अधिक पसन्द करता है। सादा भोजन कीजिए। दूध तथा फल एकाग्रता में सहायक होते हैं। भोजन को जीवन-निर्वाह के लिए औषधि के समान लीजिए। भोग के लिए भोजन करना पाप है। एक माह के लिए नमक तथा चीनी का परित्याग कीजिए। बिना चटनी तथा अचार के केवल चावल, रोटी तथा दाल पर ही निर्वाह करने की क्षमता आपमें होनी चाहिए। दाल के लिए और अधिक नमक तथा चाय, काफी और दूध के लिए और अधिक चीनी र माँगिए ।
५. ध्यान कक्ष-ध्यान कक्ष अलग होना चाहिए। उसे ताले कुंजी से बन्द रखिए।
६. दान- प्रतिमाह अथवा प्रतिदिन यथाशक्ति नियमित रूप से दान दीजिए अथवा एक रुपये में दस पैसे
के हिसाब से दान दीजिए।
७. स्वाध्याय गीता, रामायण, भागवत, विष्णुसहस्रनाम, आदित्यहृदय, उपनिषद्, योगवासिष्ठ,
बाइबिल, जेन्द अवस्ता, कुरान आदि का आधा घण्टे तक नित्य स्वाध्याय कीजिए तथा शुद्ध विचार रखिए।
८. ब्रह्मचर्य बहुत ही सावधानीपूर्वक वीर्य की रक्षा कीजिए वीर्य विभूति है। वीर्य ही सम्पूर्ण शक्ति है।
वीर्य ही सम्पत्ति है। वीर्य जीवन, विचार तथा बुद्धि का सार है।
९. स्तोत्र पाठ - प्रार्थना के कुछ श्लोकों अथवा स्तोत्रों को याद कर लीजिए। जप अथवा ध्यान आरम्भ
करने से पहले उनका पाठ कीजिए। इससे मन शीघ्र ही समुन्नत हो जायेगा।
१०. सत्संग निरन्तर सत्संग कीजिए कुसंगति, धूम्रपान, मांस, शराब आदि का पूर्णतः त्याग कीजिए बुरी
आदतों में न फैसिए।
११. व्रत — एकादशी को उपवास कीजिए या केवल दूध तथा फल पर निर्वाह कीजिए।
१२. जप माला — जप माला को अपने गले में पहनिए अथवा जेब में रखिए। रात्रि में इसे तकिये के नीचे
रखिए।
१३. मौनव्रत- नित्यप्रति कुछ घण्टों के लिए मौन व्रत कीजिए।
१४. वाणी संघम- प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलिए घोड़ा बोलिए। मधुर बोलिए। -
१५. अपरिग्रह — अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए। यदि आपके पास चार कमीजें हैं, तो इनकी
संख्या तीन या दो कर दीजिए सुखी तथा सन्तुष्ट जीवन बिताइए। अनावश्यक चिन्ताएँ त्यागिए। सादा जीवन व्यतीत कीजिए तथा उच्च विचार रखिए।
१६. हिंसा - परिहार — कभी भी किसी को चोट न पहुँचाइए (अहिंसा परमो धर्मः) । क्रोध को प्रेम, क्षमा
तथा दया से नियन्त्रित कीजिए।
१७. आत्म निर्भरता - सेवकों पर निर्भर न रहिए। आत्म निर्भरता सर्वोत्तम गुण है। १८ . आध्यात्मिक
डायरी-सोने से पहले दिन भर की अपनी गलतियों पर विचार कीजिए। आत्म-विश्लेषण कीजिए दैनिक आध्यात्मिक डायरी तथा आत्म-सुधार रजिस्टर रखिए। भूतकाल की गलतियों का चिन्तन न कीजिए।
१९. कर्तव्य पालन - याद रखिए, मृत्यु हर क्षण आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अपने - कर्तव्यों का पालन
करने में न चूकिए। सदाचारी बनिए।
२०. ईश-चिन्तन – प्रातः उठते ही तथा सोने से पहले ईश्वर का चिन्तन कीजिए। ईश्वर को पूर्ण आत्मार्पण
कीजिए।
यह समस्त आध्यात्मिक साधनों का सार है। इससे आप मोक्ष प्राप्त करेंगे।
इन नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। अपने मन को ढील न दीजिए।
विश्व - प्रार्थना
हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव!
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है।
तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ हो।
तुम सच्चिदानन्दघन हो । तुम सबके अन्तर्वासी हो ।
हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समत्व प्रदान करो।
श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो।
हमें आध्यात्मिक अन्त:शक्ति का वर दो,
जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों।
हम अहंकार, काम, लोभ, घृणा, क्रोध और द्वेष से रहित हों।
हमारा हृदय दिव्य गुणों से परिपूरित करो।
हम सब नाम-रूपों में तुम्हारा दर्शन करें।
तुम्हारी अर्चना के ही रूप में इन नाम-रूपों की सेवा करें।
सदा तुम्हारा ही स्मरण करें।
सदा तुम्हारी ही महिमा का गान करें।
तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे अधर-पुट पर हो।
सदा हम तुममें ही निवास करें।
-स्वामी शिवानन्द