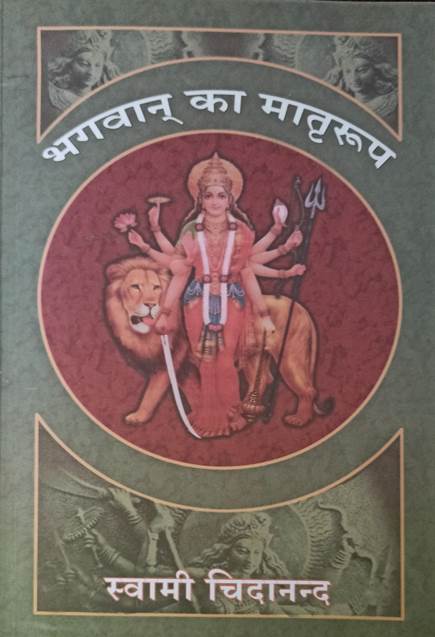
भगवान् का मातृरुप
GOD AS MOTHER
का हिन्दी अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती
अनुवादक
श्री शिवगोविन्द गुप्त, एम. ए., साहित्यरत्न
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२
जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण : १९७६
द्वितीय हिन्दी संस्करण १९९१
तृतीय हिन्दी संस्करण २००९
चतुर्थ हिन्दी संस्करण : २०१४
(५०० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
HC 3
PRICE: 70/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा
प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त फारेस्ट एकाडेमी प्रेस,
पो. शिवानन्दनगर-२४९१९२, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित ।
For online orders and Catalogue visit dlsbooks.org
अथ सप्तश्लोकी दुर्गा
शिव उवाच-
देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी ।
कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः ।।
देव्युवाच -
शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम्।
मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ।।
ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थं सप्तश्लोकीदुर्गापाठे विनियोगः ।
ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा।
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥१॥
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ।
दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ॥२॥
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥४॥
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥५॥
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा
रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥६॥
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि ।
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॥७ ॥
इति श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्णा ॥
निवेदन
करुणामयी माँ के चरण कमलों में कोटि-कोटि प्रणाम! जगज्जननी माँ की जय हो! पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती-रूपा माँ के श्रीचरणों में हमारा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण प्रणाम! वह आद्यशक्ति, पराशक्ति तथा सच्चिदानन्दमयी है। परब्रह्मस्वरूपिणी माँ काली की जय हो! शक्ति, सौन्दर्य तथा सौभाग्य-रूप में तुम स्वरूपतः परब्रह्म का ही प्रकाश हो। हे माँ! सब पर तुम्हारा आशीर्वाद हो!
'भगवान् का मातृरूप' माँ के चरणों में निवेदन करते हुए मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव करता हूँ। यह तो माँ की ही वस्तु है। कारण, माँ की दया और करुणा के बिना किसी भी मानव की बुद्धि में प्रकाश आना सम्भव नहीं है। यदि इस पुस्तक में अन्तर्निहित तत्त्व तथा उच्च भाव हमारे मन को उत्साहित करें, तो यह पूजा और भी सुन्दर हो सकती है।
श्री भगवती माँ सम्पूर्ण सृष्टि में अन्तर्निहित प्राण-शक्ति हैं। वही सब जीवों की अन्तरात्मा हैं। अतः माँ की श्रेष्ठ पूजा है सभी मानवों की श्रद्धान्वित सेवा, जीवों के प्रति श्रद्धा, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया। निस्सन्देह, माँ की प्रतिमा अथवा पट पर पूजा की भी आवश्यकता है, तथापि माँ की पूजा का यह भी एक अंग है, और अत्यावश्यक अंग है। तभी पूर्ण भाव से और श्री माँ के मन की भावनाओं के अनुसार पूजा होगी। सभी प्राणियों में माँ की उपस्थिति अनुभव तथा उपलब्ध करनी होगी और जिस भाव से माँ की सेवा करते हैं, उसी भाव से सभी प्राणियों की सेवा करनी होगी।
श्री श्री माँ की पूजा का प्रधान अंग है सब जीवों के प्रति श्रद्धा, सम्मान तथा प्रीति-प्रदर्शन। माँ हमारे भक्ति के अर्घ्य को तभी स्वीकार करेंगी, जब हम उनकी समस्त सन्तानों के प्रति समदृष्टि रखेंगे और करुणापूर्ण व्यवहार करेंगे। उनकी सन्तान को कष्ट या दुःख दे कर हम कभी भी माँ को सन्तुष्ट नहीं कर सकते। समस्त मानव उनकी ही सन्तान है। समग्र सृष्टि, यहाँ तक कि पशु-पक्षी भी उनकी ही सन्तान हैं। कोई भी उनकी गोद से बाहर नहीं है। कोई उनसे विलग नहीं है। अतः सबके कल्याणकारी बनो। सबका आलिंगन करो। सबमें माँ का दर्शन करो। उनकी सन्तान की सेवा करके माँ की सेवा करो। सामान्य तृण, पुष्प या तितली को भी आघात न पहुँचाओ। करुणाशील बनो। जीव मात्र के प्रति करुणापूर्ण व्यवहार करो। कभी किसी को आहत न करो। पीड़ितों की सेवा करो। दरिद्रों की सेवा करो। आर्तो की सेवा करो। शोक-ग्रस्तों को सान्त्वना प्रदान करो। दुःखियों को शान्ति दो। असहायों को साहाह्य प्रदान करो। आश्रयहीनों को आश्रय दो। दुर्बलों को साहस यो। सहायहीनों से आश्वासनप्रद वार्ता करो। यही महिमामयी माँ की श्रेष्ठ पूजा है।
सदा स्मरण रखो कि मानव भगवान् का चल-मन्दिर है। इसका अनुभव करना ही जीवन्त तथा वास्तविक पूजा है। माँ सर्वत्र विद्यमान है। अतः माँ की सर्वत्र, सभी जीवों में पूजा करो। यही माँ की सच्ची पूजा है।
देवीसूक्त का पाठ करने से यह रहस्य सहज ही समझ में आ जायेगा कि वह ही अन्दर, बाहर सभी वस्तुओं में तथा सभी वस्तु-रूप में विराजती है।
यहाँ अति-संक्षेप में माँ की कृपा से उस करुणामयी माँ के विश्वव्यापी रूप तथा उनकी पूजा के तत्त्व को किंचित् विस्तार से प्रकाश में लाने की चेष्टा की गयी है। यहाँ साधक के वैयक्तिक जीवन में मातृ-शक्ति के उद्दीपन में अन्तर्निहित नैतिक तथा आध्यात्मिक भाव पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गयी है। आशा है कि अपने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने में साधक को यह ग्रन्थ उसके जीवन में सहायक होगा।
यह कोई तन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ नहीं है और न शाक्त मत की व्याख्या ही है। यह तो मातृ-पूजा तथा माँ की भक्ति की यौगिक व्याख्या कही जा सकती है। प्रेम-दृष्टि से, योग-दृष्टि से माँ के प्रति सभक्ति दृष्टिपात है। हमारे धार्मिक तथा राष्ट्रीय जीवन की जागृति में साहाय्य होने के लिए श्री माँ का भक्तिपूर्ण आह्वान है। मैं अति विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ कि यदि जन-साधारण इस पुस्तक को सभी ग्रन्थालयों, पाठशालाओं, महाविद्यालयों तथा सत्संगों और वाचनालयों में स्थान दे कर सर्वसाधारण के अध्ययनार्थ उपलब्ध करने की व्यवस्था करेंगे, तो सबका विशेष उपकार होगा।
गृह में माता-पिता इस पुस्तक का पाठ करें। पाठ के समय अपनी सन्तान को भी इसका भावार्थ अवगत करा दें, इस प्रकार की आलोचना से वह मांगल्य को प्राप्त करेंगे। दुर्गा-पूजा-काल में इसे पूजा की कर्म-सूची में स्थान दे सकते हैं। वर्तमान पत्रों में भी इसका प्रचार तथा प्रसार कर सकते हैं। इसके पुनर्मुद्रण में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं; क्योंकि इसका रचयिता मैं हूँ, ऐसा मेरे मन में किंचित् भी भाव नहीं है। यह मेरी रचना नहीं, माँ की रचना है। माँ इस पुस्तक के माध्यम से अपनी अपार महिमा का अति अल्पांश हम अकिंचनों पर दया करके स्वयं प्रदान कर रही हैं। यह सब माँ का दान है, माँ की ही महिमा है, माँ का ही ऐश्वर्य है।
प्रिय पाठक! इस पुस्तक में निहित माँ की करुणामयी कृपा आपके जीवन में विकसित हो! आपको दिव्य ज्योति, शक्ति एवं ज्ञान प्राप्त हो! माँ आपको स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, श्री, साफल्य, विश्वास, भक्ति तथा श्रेष्ठ आध्यात्मिक आनन्द प्रदान करें!
आप शान्ति, आनन्द तथा अमृतत्व प्राप्त करें! जै माँ भगवती! ॐ तत्सत्।
माँ का चरणाश्रित
स्वामी चिदानन्द
भूमिका
परमात्मा के साथ जीव के गूढ़ सम्बन्ध पर विचार करने से परमेश्वर का मातृ-भाव हमारी हृदय-गुहा में स्वतः ही स्फुरित हो उठता है। इस मानव-शरीर के आधार में आध्यात्मिकता का सापेक्षिक विकास निरन्तर होता रहता है। व्यक्ति के अध्यात्म की एक भावधारा में पहुँचने पर दिव्य शक्ति, माया अथवा अन्य नाम वाली कोई दैवी प्रकृति उससे उच्चतर भावधारा की प्राप्ति का माध्यम बनती है। भगवती माँ की आराधना भगवत्प्राप्ति की प्रचेष्टाजन्य सुगम्भीर अनुभूति में सहायक होती है।
यद्यपि इस देश में मातृभावाश्रित पूजा-पद्धति तथा भावधारा युग-युगान्तरों से प्रचलित है, तथापि इस भावधारा का भावबोध हमारे धर्मपिपासुओं को अब अगोचर है। नाना प्रकार के बाह्य अनुष्ठान, वीभत्सता, लम्पटता आदि पूजांगों ने शताब्दियों से मातृ-पूजा की पद्धति को विकृत कर दिया है तथा शृंगार के आचार-विचार भी व्यभिचार में पर्यवसित हो गये हैं। इसी कारण अब मातृभावापन्न पूजा-पद्धति को पुनः प्रतिष्ठित करने की नितान्त आवश्यकता है। इस दृष्टि से वर्तमान समय में 'भगवान् का मातृरूप' पुस्तक का प्रकाशन विशेष रूप से समयोपयोगी तथा जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होगा।
आशा है, इस ग्रन्थ से सत्यान्वेषी साधक-समुदाय विशेष उपकृत होगा।
-द डिवाइन लाइफ सोसायटी
ॐ ह्रीं ॐ
आत्मार्पण
जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचनं
गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः ।
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदशा
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम् ।।
काव्यानुवाद :
जो बोलूँ सो मन्त्र-जाप है, जो कुछ करूँ सो सेवा ।
चलना-फिरना तव परिक्रमा, आहुति खाद्य कलेवा ॥
सो जाना ही नित्य दण्डवत्, सुख आत्मार्पण देवा।
हों स्वीकार कर्म सब मेरे, क्रम पूजा सम लेवा ॥
विषय-सूची
प्रथम रात्रि
द्वितिय रात्रि
तृतीय रात्रि
जीवन के मध्य में ही ध्वंस की क्रीड़ा रहती है
अपने अन्दर के पशु-भाव की बलि दो
आध्यात्मिक साधना में दुर्गा का प्राकट्य
चतुर्थ रात्रि
पंचम रात्रि
राष्ट्रीय नेताओं का सर्वोपरि कर्तव्य
षष्ठ रात्रि
गृह तथा हृदय में सौभाग्यदायिनी देवी
गृह में लक्ष्मी जी का आविर्भाव
सप्तम रात्रि
जिस दिव्य ज्योति के प्रकाश से अन्धकार दूर होता है
अष्टम् रात्रि
नवम् रात्रि
स्वाध्याय तथा उसका व्यावहारिक मूल्य
विजय दशमी
गुरु : परब्रह्म की स्थूल मूर्ति
महान् धर्मशास्त्रों का सारतत्त्व
परिशिष्ट
श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती(जीवन-झांकी)
प्रथम रात्रि
ॐनमश्चण्डिकायै
पराशक्ति का अलौकिक प्रकाश
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।।
(दुर्गासप्तशती : ५-१६)
(विष्णु की माया कहलाती जो व्याप्त सर्वभूतों में माँ।
नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, उसे नमः ।।)
समस्त सृष्टि की उद्भव, स्थिति तथा संहारकारिणी भगवती परम कल्याणमयी माँ के श्रीचरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम!
चिन्मयी माँ ब्रह्म की ही अलौकिक अव्यक्त शक्ति हैं। ब्रह्म असीम, अनन्त और अनिर्वचनीय परम शान्ति है। वह इन्द्रिय व मन से अनधिगम्य है। माँ उसी परब्रह्म का ही गतिशील रूप हैं।
नवरात्र की प्रथम रात्रि से आरम्भ हो कर जो विजयादशमी को समाप्त होता है और जो साधारणतः दशहरा तथा दुर्गा-पूजा के नाम से प्रसिद्ध है, उस वार्षिक पवित्र नवरात्र-पूजा के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ प्रथम दिवस को एकत्रित हो कर माँ की आराधना में निरत हैं। निश्चय ही यह भगवती माँ की कृपा का महान् संकेत है। जिनकी कृपा से जागतिक व पारमार्थिक, आध्यात्मिक व व्यावहारिक सभी प्रचेष्टाओं में सफलता व सिद्धि प्राप्त होती है, जिनकी दया से साधक अपनी साध्य वस्तु को उपलब्ध करने में समर्थ होता है, जिनके अनुग्रह से जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा का समाधान पा लेता है, जीवात्मा पूर्णता को प्राप्त कर भूमा का साक्षात्कार कर पाता है, आज उनके सम्बन्ध में अल्प शब्दों में कुछ चर्चा करने के लिए, उनका पूजा-पाठ, स्तव-स्तुति करने के लिए एकत्रित हुए हैं, यही परम सौभाग्य है। माँ की कृपा के बिना सिद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज के इस पवित्र क्षण में हम भगवती माँ के सम्बन्ध में भारतीय विचारधारा तथा इस नवरात्र-पूजा के मर्म व ऐतिह्य जानने की कुछ चेष्टा करेंगे।
भारतीय हिन्दुओं की उपासना साधारणतया चार बा पाँच विभिन्न धाराओं में विभक्त है। जो भगवान् की शिव-रूप में उपासना करते हैं, वे 'शैव' कहे जाते हैं। उसी भगवान् की जो विष्णु-रूप में उपासना करते हैं, उन्हें 'वैष्णव' कहते हैं। एक तृतीय प्रकार के उपासक है जो उस एक ही भगवान् की देवी-शक्ति के रूप में आराधना करते हैं, वे 'शाक्त' कहलाते हैं। इनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इनके अतिरिक्त दो कुछ कम प्रसिद्ध विभाग हैं जो 'गाणपत्य' तथा 'सौर्य' के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान् की गणपति-रूप में उपासना करने वालों को 'गाणपत्य' कहते हैं तथा सूर्य-मण्डल के प्रत्यक्ष तेज-रूप, इस लोक के प्रकाशक और जीवन-गति को धारण करने वाले सूर्य के रूप में भगवान् की उपासना करने वालों को 'सौर्य' कहा जाता है।
नवरात्र की देवी-उपासना मुख्यतः शाक्त-उपासना है और इसकी पद्धति हमें शाक्त-परम्परा से ही प्राप्त हुई है। बंगाल तथा असम में बहुत से लोग इसी भावधारा से उपासना करते हैं। 'दुर्गासप्तशती' अथवा 'देवी-माहात्म्य' इनकी प्रधान तन्त्र-पुस्तक है। इसमें सात सौ श्लोक हैं। इसी कारण इसे 'सप्तशती' कहते हैं। बंगाली भाषा में इसका नाम 'चण्डी' है तथा गढ़वाल में भी देवी-माहात्म्य-पाठ को 'चण्डी-पाठ' कहा जाता है। कारण, माँ 'चण्डिका' नाम से भी प्रसिद्ध हैं।
यह चण्डी-पाठ खूब नियम व निष्ठापूर्वक किया जाता है। शास्त्रों में इसके पाठ का नियम बहुत ही विधि-विधानपूर्वक दिया गया है। प्रथम अंश में, जिसका आज पाठ किया गया है, देवी-तत्त्व की विशद आलोचना है। इसकी योजना एक कथानक के रूप में है। एक ब्रह्मज्ञ ऋषि ने एक राजा और एक वैश्य को देवी के माहात्म्य की व्याख्या की है। देवी कौन हैं, उनका स्वभाव क्या है, वह स्वरूपतः क्या हैं, देवी-सम्बन्धी इन सब गम्भीर दार्शनिक तथ्यों से यह परिपूर्ण है। इसमें सुन्दर प्राणस्पर्शी महान् स्तव दिये गये हैं, देवी-पूजन की विधि दी गयी है। शाक्त-उपासना-विधि में चण्डी का आद्योपान्त पाठ ही एक महान् तथा प्रभावशाली साधना है। यहाँ मैं इस ग्रन्थ का मूल विषय संक्षेप में दे रहा हूँ।
देवी-माहात्म्य का सार
देवी-माहात्म्य इस प्रकार आरम्भ होता है। श्री रामचन्द्र के सूर्यवंश में सुरथ नामक एक राजा हुए। एक बार अपने शत्रुओं द्वारा आक्रान्त व पराजित होने पर राज्य त्याग कर पलायन करने को वे बाध्य हुए। उन्होंने अरण्य का आश्रय लिया। धन व जन सब-कुछ छिन जाने के कारण वे बहुत ही क्लेशित व विषण्ण थे और इस दुर्दशाग्रस्त अवस्था में एकाकी विचरण करते फिरते थे। उनके मन में पुनः पुनः अपने नष्ट राज्य व हतभाग्य का विचार उठता। अपने राज्य, अपनी सम्पत्ति व अपने मन्त्रियों के विषय की चिन्ता उनके मन में उदित होने लगी तथा नूतन राजा इस समय कैसे राज्य-शासन करता होगा, इस चिन्ता में मग्न रहने लगे। जब उनकी यह मनोदशा थी, उस समय वह मेधा नामक एक ब्रह्मज्ञ ऋषि के आश्रम के सन्निकट पहुँचे। वह इस आश्रम के सौन्दर्य, शिष्य-कुल और इसके गम्भीर, प्रशान्त व पवित्र परिवेश से आकृष्ट हो कर वहीं रहने लगे।
इस आश्रम में रहते हुए संयोगवश उनकी समाधि नामक एक वैश्य से भेंट हुई। वह भी उनके समान ही दुर्दशाग्रस्त था और दुर्भाग्य के कारण घर से भाग निकला था। उसकी सारी सम्पत्ति उसके सम्बन्धियों, स्नेहियों तथा कुटुम्बी जनों ने छीन ली थी और उसे घर से निष्काषित कर दिया था। वह भी अपने परिजनों से विताड़िता हो कर इस वन में विचरण करता था और मुनि के चरणों का आश्रय ग्रहण किये था।
उन दोनों ने देखा कि वे दोनों एक-सी ही विषम स्थित में हैं। यद्यपि उनके निजी आत्मीय जनों ने उनका सर्वस्व अपहरण कर उन्हें उनके गृह से निष्काषित कर दिया है, उनके परिजन ही उनके शत्रु और विरोधी बन गये हैं, तथापि उनका मन उन सब लोगों की चिन्ता में ही मग्न रहता है। यह उनके लिए अति आश्चर्य तथा उलझन का विषय है कि जिन लोगों ने उन्हें विताड़ित किया है, जो उनके सम्पूर्ण दुःखों के कारण हैं और जिन वस्तुओं से उनके सम्पूर्ण कष्टों की उत्पत्ति हुई, जिनसे उन्हें निराशा और उदासी झेलनी पड़ी, उनका मन पुनः पुनः उन्हीं लोगों तथा उन्हीं वस्तुओं का चिन्तन करता रहता है।
वे दोनों परस्पर आलोचना करने लगे कि मन का यह कैसा अद्भुत स्वभाव है कि जो लोग तथा वस्तुएँ सम्पूर्ण दुःख तथा शोक का कारण हैं, उन्हें जान कर भी वह उन लोगों में आसक्त रहता है और उन्हीं वस्तुओं के प्रति सदा आकृष्ट होता है। इस समस्या का कोई समाधान न पा कर वे दोनों इसके समाधान के लिए ऋषि मेधा के पास विनीत भाव से गये। उन्होंने ऋषि से कहा- "हे ज्ञानी प्रवर! इस विषय पर आप कुछ प्रकाश डालें। हमें यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन वस्तुओं से हमें दुःख तथा ग्लानि प्राप्त हुई है और जिन लोगों ने हमें सब प्रकार का कष्ट दिया है, यह मन सदा उन्हीं वस्तुओं की ओर आकृष्ट रहता है और उन्हीं लोगों के प्रति अत्यन्त आसक्त रहता है। मन जानता है कि इन सम्पूर्ण वस्तुओं में कोई सुख नहीं है, तथापि वह इनकी आसक्ति का त्याग नहीं कर पाता। मन के इस प्रकार के मोह का कारण क्या है, कृपा करके बतलाइए।”
राजा सुरथ और वैश्य समाधि के ये प्रश्न वस्तुतः सारे जगत् के प्रश्न हैं तथा प्रत्येक चिन्तनशील मानव का मन इन प्रश्नों से उद्वेलित रहता है। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि मेधा ने देवी-माहात्म्य की एक अपूर्व व्याख्या दी है। उन्होंने कहा- "बालको! मानव-मन एक आश्चर्यमयी माया के द्वारा बद्ध है, जिससे उसकी विशुद्ध विचार-शक्ति तमसावृत हो रही है। उससे ही उसका मन पुनः पुनः सब प्रकार के दुःख तथा बन्त्रणा के कारण-रूप सम्पूर्ण वस्तुओं व व्यक्तियों में आसक्त हो कर बार-बार उनमें ही विचरण करता है। यह माया, यह आवरण-शक्ति वस्तुतः महामाया की ही अलौकिक शक्ति है। वही यह विश्वमाया हैं। इस विश्व-प्रपंच के पृष्ठ देश में वही रहती है। उनकी ही रहस्यमयी आवरण-शक्ति एक को अनेक करके दिखाती है, अरूप को बहुरूप धारण कराती है और अव्यक्त को व्यक्त करती है। यह उस ब्रह्म की ही अवर्णनीय शक्ति है। यही ब्रह्म-शक्ति है। यही महामाया भगवान् की विश्वव्यापी विमोहिनी-शक्ति है जो स्वयं भगवान् से प्रकट हुई है। इसी शक्ति के द्वारा वह अपने जगत्-नाटक के नाम-रूपों की सृष्टि, स्थिति व प्रलय कर पुनः अपने विशुद्ध परमात्म-स्वरूप में अन्तर्लान कर लेते हैं।"
राजा सुरथ तथा वैश्य समाधि में ऋषि द्वारा वर्णन की गयी इस अलौकिक शक्ति के सम्बन्ध में अधिक जानने की जिज्ञासा हुई। विश्व-प्रपंच के पृष्ठ भाग में स्थित हो कर जो उसका संचालन करती है, उस विश्वमाया के विषय में उन्होंने सविस्तार जानना चाहा। उनके अनुरोध पर मेधा ऋषि ने महामाया के स्वरूप की कथा विस्तृत रूप से बतलायी। सप्तशती में इसी का वर्णन है। अन्त में महामाया के देवी-भाव और उनके अलौकिक रहस्य की व्याख्या करके ऋषि ने सुरथ और समाधि को योगाभ्यास द्वारा देवी की पूजा, ध्यान व आराधना करके माँ को तुष्ट करने का परामर्श दिया। इस भाव से आराधना करने पर माँ उनके सम्मुख प्रकट हुईं, उन पर अपनी कृपा-वृष्टि की और उनकी मनोवांछा पूर्ण की।
यही शाक्तों के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र देवी-माहात्म्य ग्रन्थ का सारांश है।
माया और ब्रह्म एक ही हैं
देवी-तत्त्व की इस व्याख्या से पता चलता है कि वह परमा शक्ति ही सर्वेसर्वा हैं। इसमें कहा गया है कि इस परिदृश्यमान् जगत्-प्रपंच में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब परब्रह्म की पराशक्ति की क्रिया है। उसे ही आदिशक्ति कहते हैं। उसे ही पराशक्ति कहते हैं। उसे ही श्रेष्ठ विराट् शक्ति और महाशक्ति कहते हैं।
उस सर्वशक्तिमान् परमात्मा के साथ इस महाशक्ति का क्या सम्बन्ध है, यह एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है और यह प्रश्न प्रायः सभी महान् विचारकों के मन में उठा करता है। इस सम्बन्ध में अनेकों व्याख्याएँ सुनने में आती हैं; किन्तु तत्त्वज्ञानी ऋषियों ने इस गम्भीर गूढ़ तत्त्व के विषय की, भगवान् के इस अलौकिक (परब्रह्म) रूप और उनके महामायिक पराशक्ति-रूप के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय की स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। वे कहते हैं कि परब्रह्म और जगत् को आवरण करने वाली अचिन्त्य माया शक्ति या देवी तत्त्वतः एक ही वस्तु हैं। बाह्यतः उनमें पार्थक्य प्रतीत होते हुए भी मूलतः एक ही हैं, कार्यतः पृथक् दृष्टिगोचर होते हुए भी आन्तरिक रूप से एक ही हैं। यही अभेद में भेद है। यही उनमें सम्बन्ध है मानो एक ही सिक्के के मुख व पृष्ठ दो रूप हों। महामाया को छोड़ कर परब्रह्म की भावना नहीं की जा सकती एवं परब्रह्म की भावना करते ही उनकी शक्ति महामाया की भावना करनी होती है। वे बतलाते हैं कि महामाया ने ही व्यक्त और अव्यक्त को संयोजित कर रखा है। वही व्यक्त और अव्यक्त को जोड़ने वाली श्रृंखला है। जिस प्रकार कार्य और उसका एक कारण होता है, किन्तु इनको संयोजित करने वाला सूत्र क्या है? इनके मध्य एक रहस्यमय योगसूत्र है, जो इन्हें परस्पर एकीभूत बनाये रखता है। यद्यपि देखने में दो लगते हैं, किन्तु वस्तुतः वे एक ही धारा के दो छोर हैं। जिस शक्ति के द्वारा कार्य कारण के रूप में प्रकट होता है एवं कारण व कार्य संयुक्त रहते हैं, वही माया अलीक प्रपंच अथवा देवी है।
परब्रह्म निश्चल व निष्क्रिय है; क्योंकि वह असीम है, अनन्त है, अतः उसमें किसी गति या क्रिया का प्रश्न का ही नहीं उठता। पराशक्ति, जिसे हम देवी कहते हैं, वही परब्रह्म का सक्रिय भाव है। जिस प्रकार दुग्ध तथा उसकी शुभ्रता, अग्नि और उसकी दाहिका-शक्ति, सर्प और उसकी तिर्यक् गति परस्पर अभिन्न हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और उसकी शक्ति भी अभिन्न हैं। दुग्ध का विचार आते ही उसकी शुभ्रता का भी विचार मन में आता है, अग्नि का विचार आते ही उसकी दाहिका-शक्ति का विचार भी मन में आता है। जिस प्रकार अग्नि से उसकी दाहिका-शक्ति निकाल लेने पर वह अग्नि नहीं रह जाती, उसी प्रकार परब्रह्म और उसकी शक्ति अभिन्न हैं। यदि ब्रह्म अग्नि है, तो शक्ति या देवी अग्नि की दाहिका-शक्ति है।
ब्रह्म तथा माया या प्रकृति या शक्ति के मध्य के गूढ़ सम्बन्ध को समझाने के लिए एक आधुनिक उदाहरण भी दिया जा सकता है। वह उदाहरण है विद्युत् उत्पादन करने वाला यन्त्र (बैटरी) तथा उसके मध्य की विद्युत्-शक्ति। जिस समय वह यन्त्र क्रियाशील नहीं होता है, स्थिर होता है, उस समय इसको इधर-उधर ले जा सकते हैं। उस समय कोई यह नहीं जान सकता है कि उसके मध्य में इतनी विराट् शक्ति गुप्त रूप से भरी पड़ी है। वहाँ हमें ऐसा कोई बाह्य लक्षण भी दृष्टिगोचर नहीं होता कि जिससे यह कल्पना की जा सके कि उसमें इतनी अद्भुत शक्ति समाहित है। किन्तु विद्युत् तन्तु-प्रणाली द्वारा, परिपथ द्वारा जिस समय यह विद्युत्-यन्त्र (बैटरी) अद्भुत रूप से क्रियाशील हो उठता है, उस समय इसकी निश्चल शक्ति सचल हो उठती है। स्थाणु भाव के जाते रहने पर विराट् कर्मरत शक्ति की क्रिया प्रकट हो उठती है। यह विद्युत् के समान गतिशील होती है। स्पर्श करने पर झटका देती है। ज्योति विकिरण कर उद्दीप्त हो उठती है और आलोक, प्रकाश करती है। चक्रगति से पंखे को चलाती है। कभी यह प्रचण्ड शैत्यधार यन्त्र (रेफ्रीजरेटर) में हिम की सृष्टि करती है और अँगीठी (हीटर) के अन्दर प्रचण्ड अग्नि की सृष्टि करती है। नादयन्त्र (सायरेन) के मध्य में तुमुल नाद की सृष्टि करती है। बैटरी के बीच में जो शक्ति स्थाणु भाव से थी, वही जब गतिशील होती है तो आलोक, गति, ताप, शीत, नाद आदि अनेक प्रकार से हमारी इन्द्रियों के ग्राह्य भाव से प्रकट होती है। इसी भाँति उसी पराशक्ति को अव्यक्त, अक्रिय, स्थाणु अवस्था में परब्रह्म अथवा नाम-रूप-गति-हीन परम अव्यक्त कहते हैं और वही जब गतिवान् सक्रिय भाव धारण करती है, सृष्टि कर नाम-रूप धारण करती है, सारे विश्व-ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो कर प्रकट होती है, उस समय उसे महामाया करते हैं। दोनों एक ही हैं।
महामाया ही विद्युत्-शक्ति, सूर्य की आभा, सागर की गम्भीरता, हाथ की गति, कुसुम का सौरभ, शब्द की स्वर लहरी, इस ब्रह्माण्ड के समस्त दृश्य व अदृश्य पदार्थ, सम्पूर्ण गतिशील की गति तथा सभी प्रकार की शक्ति हैं। वही मानव-चित्त में बुद्धि-रूप में, मन-रूप में, वृत्ति-रूप में तथा भाव-रूप में अवस्थित हैं। हमें जो भी प्रत्येक व्यक्ति के अन्तर व बाह्य प्रकृति में क्रिया-शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है, वह सब वही हैं। वही विश्व की प्राण हैं। वही विश्व की उत्पत्ति, स्थिति व लय की कारण हैं। 'सर्व शक्तिमयं जगत्।' यही परम सत्य है। इस विश्व में स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक, क्षुद्रतम से ले कर बृहत्तम तक जो कुछ भी वर्तमान है, वह सब ही उसी महामाया का प्रकाश अथवा परब्रह्म की अलौकिक शक्ति का विकास है। यह पराशक्ति ही सब नाम-रूपों में प्रकाशित है, सम्पूर्ण प्रकाशों का मूल व व्यक्त का आदि है। माया के कारण यह व्यक्त भाव सम्भव हो सका है।
इन नौ दिनों में हम इस पराशक्ति की विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं। इस पराशक्ति के भावुक भक्त जन इसे तीन विशेष भावों में महाकाली अथवा दुर्गा, महालक्ष्मी और
महासरस्वती के रूप में पूजा करते हैं। नौ दिनों को तीन-तीन दिनों में तीन भागों में विभाजित किया है। प्रथम तीन दिनों में देवी की महाकाली या दुर्गा के रूप में, द्वितीय तीन दिनों में महालक्ष्मी के रूप में एवं अन्तिम तीन दिनों में महासरस्वती के रूप में कल्पना कर पूजा करते हैं। इस भाव से पर-अपर तीन रूपों में माँ की कल्पना व पूजा का गम्भीर महत्त्व व विशेष उद्देश्य है। इसके विषय में हम आगामी दिवसों में विचार करेंगे।
द्वितीय रात्रि
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे
अशुभ शक्ति-विनाशिनी
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।।
(दुर्गासप्तशती ५-३४)
जो देवी है शक्ति-रूप से व्याप्त सर्वभूतों में माँ।
नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है उसे नमः ॥
परब्रह्म की अलौकिक, अचिन्त्य तथा दुर्बोध शक्ति उस कल्याणमयी परमा माता को बार-बार प्रणाम! जिससे इन असंख्य ब्रह्माण्डों का आविर्भाव होता है, जो असंख्य प्रकाशों का अवस्थान है तथा सम्पूर्ण नाम व रूप जिसके मध्य में लय हो कर परब्रह्म में मिल जाते हैं, उस दिव्य शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ।
परब्रह्म की मातृ-रूप में भावना करने का कारण सहज ही जाना जा सकता है। कारण, इस संसार में जन्म ग्रहण करने वाले प्रत्येक प्राणी को प्रथम ज्ञान अपनी माँ का ही होता है। जीव को अपने प्रारम्भिक जीवन की सर्वप्रथम स्मृति यदि कुछ हो सकती है, तो वह है माँ के अंक में शयन करते हुए उसके वात्सल्यपूर्ण नेत्रों की ओर एकटक देखते रहने की स्मृति। शिशु के लिए अखिल विश्व की कोमलता, करुणा, पोषण व पालन का विषय अपनी माँ में घनीभूत व केन्द्रीभूत रहता है। यहाँ ही उसका आदर्श जगत् है, जहाँ से वह अपनी जीवनी शक्ति प्राप्त करता है, सुख के लिए जिधर भागा जाता है तथा रक्षा और परिपोषण के लिए जिससे चिपटा रहता है। वहीं पर वह अपने सुख, निर्भयता, आश्रय की वस्तु को खोज पाता है। कारण, सहृदयता, यत्न तथा निर्भयता की आदर्श भूमि माँ है। इसीलिए सृष्टिकर्ता में यह धारणा व आदर्श आरोपित करने का विचार बहुत ही स्वाभाविक, युक्ति-युक्त व सहज बोधगम्य है। इसी कारण हिन्दू-दर्शन में इस महिमान्वित जगन्माता की भावना का उद्भव हुआ जो विश्व के सम्पूर्ण प्राणियों पर स्नेह रखती हैं, सँभाल करती हैं तथा पालन व रक्षा करती हैं।
आज हम उसी माता के महिमामय कुछ रूपों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कह कर माँ के श्रीचरणों में अपनी परम भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ भी हमें यह स्मरण रखना होगा कि उनकी पूजा करने का, उनकी महिमा का कीर्तन करने का तथा उनके महान् भाव के विषय में आलोचना करने का जो सुयोग हमें प्राप्त हुआ है, वह भी उनकी दया व कृपा से ही सम्भव हुआ है। उनकी कृपा के बिना उनके विषय में सोचना, उनका स्मरण करना, उनका चरित्र-गान करना, उनका महिमामय नाम लेना अथवा उन्हें माँ कह कर पुकारना सम्भव नहीं है। माँ परम दयामयी व अपार करुणामयी हैं। वह स्वभाव से ही प्रेममयी हैं और इसी कारण उन्होंने आज के इस शुभ और पवित्र दिवस को मन व वाणी द्वारा उनकी महिमा का कीर्तन करने का परम सौभाग्य व आनन्द प्रदान पर हमें कृतार्थ किया है।
जो-कुछ है, सब माँ है। परब्रह्म सत्स्वरूप अस्तित्व का सार है और जो-कुछ हम जानते हैं, वही माँ है। जो ज्ञान के परे है, वही पुरुष अथवा परब्रह्म है। जो-कुछ हमारे मन व इन्द्रियों द्वारा अवगत होता है, वही माँ का रूप है। हमारे बुद्धिगम्य यह विश्व मात्र ही माँ का स्वरूप नहीं है- यह क्षुद्र पृथ्वी व असंख्य चन्द्र, सूर्य, ग्रह, तारा, भू-मण्डल, आकाश-मण्डल, चन्द्र मण्डल व सूर्य-मण्डल जिसे यह विश्व कहते हैं, वे सब माँ के असीम तथा अनन्त विराट्र रूप के अति क्षुद्रतम अंश मात्र हैं। उनके मध्य इस प्रकार के कितने ही विश्व उत्पन्न होते तथा लय को प्राप्त होते हैं। माँ सर्वशक्तिमयी हैं। इस सृष्टि के पृष्ठ भाग में वही हैं। वही सब प्रकाशों का प्रथम व आदि कारण हैं। वह इस सृष्टि की ही नहीं, इस सृष्टि के सर्जक, पालक तथा संहारक की भी स्रष्टा हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर भी माँ के मध्य में अवस्थित हैं। वे असंख्य ब्रह्माओं, असंख्य विष्णुओं तथा असंख्य महेश्वरों की माँ हैं। वह जिस प्रकार सर्वशक्तिमान् हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण शक्ति उनका खेल है। इस कारण से क्रियमाण त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदिशक्ति-रूपी उनकी ही मूर्तियाँ हैं। वही सरस्वती मूर्ति से ब्रह्म-शक्ति रूप में, लक्ष्मी-मूर्ति से विष्णु-शक्ति रूप में और पार्वती-मूर्ति से शिव-शक्ति रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होती हैं।
माया और मुक्ति
सर्वशक्तिरूपिणी माँ के दो रूप हैं। हिन्दू इन दोनों भावों में उनकी पूजा करते हैं। ये भाव बड़े ही सुन्दर हैं। इनके अन्दर कितनी गम्भीर व्यंजना निहित है। माँ के ये दो रूप हैं-विश्वमोहिनी आवरणी माया तथा आवरण-उन्मोचिनी मुक्तिदायिनी महामाया। वे सबको अपने अलौकिक मायिक जगज्जाल में बद्ध कर उन्हें अपने सहज क्रीड़ा-भाव से जन्म-मृत्यु के प्रवाह में डाल देती हैं। उस समय उनको अविद्या कहते हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतिकूल है। वही परम मुक्तिदात्री भी हैं। अपने इस रूप में वह अपने बच्चों को देख कर मुस्कराती हैं और उन्हें अपने अविद्या-रूप से छुटकारा देती हैं। इस रूप में माँ विद्या माया कहलाती हैं। शिल्पियों ने परम ज्योतिर्मयी मूर्ति के रूप में उनकी कल्पना की है। उनके एक हाथ में पाश है जिसके द्वारा वह बाँधती हैं, दूसरे हाथ में एक तीक्ष्ण कृपाण है जिसके द्वारा वह अपने भक्तों के बन्धन को काट कर मुक्त बना देती हैं। इस भाँति वह विद्या माया और अविद्या माया की अलौकिक युग्म मूर्ति हैं। इसीलिए उन्हें अनिर्वचनीया कहते हैं।
माता जी इन दोनों ही भावों में इस विश्व-प्रपंच की स्रष्टा हैं। माँ के भक्त जन जिन्होंने उनकी पूजा द्वारा उनकी कृपा प्राप्त की है और जो उनके स्वरूप की उपलब्धि करने में सक्षम हुए हैं, उन्होंने प्रेमपूर्वक माँ और उनकी लीला का बड़े ही गूढ़ भाव से चित्रण किया है। हम सब जानते हैं कि जब कभी बच्चे एकत्रित होते हैं, तभी उनमें खेल की इच्छा हो उठती है एवं क्या खेल करें, यह निश्चय न कर सकने पर बूढ़ी दादी के पास जा कर उनसे जिज्ञासा करते हैं। वह भी आनन्दपूर्वक एक खेल बतला देती हैं और इस प्रकार आँख-मिचौनी का खेल आरम्भ हो जाता है। वह कहती है-"जाओ बालको, खेल आरम्भ करो।" बच्चे खेलने लग जाते हैं। वे भागते हैं, एक-दूसरे की धर-पकड़ करते हैं और आँख मिचौनी का खेल चलता रहता है; किन्तु जब कोई शिशु थक जाता है और खेल नहीं खेल सकता, उसे अब और धर-पकड़ अच्छी नहीं लगती, तो उसे बूढ़ी दादी के पास भाग कर उन्हें छू देना होता है। जो एक बार बूढ़ी दादी को छू देता है, उसे और कोई पकड़ नहीं सकता। खेल में जिस प्रकार वह वृद्धा ही उस खेल को आरम्भ करती है, खेल की प्रगति भी देखती है और खेलने वाले बच्चों के ऊपर दृष्टि भी रखती है। उनका स्पर्श कर लेने पर खेल समाप्त हो जाता है और स्पर्श करने वाले को छुट्टी मिल जाती है। उसी प्रकार यह विश्व भी माँ महामाया के लिए बच्चों का खेल है। जब कोई व्यक्ति इस दृश्य इन्द्रियग्राह्य भोग-जगत् की दौड़-धूप से क्लान्त हो कर निवृत होने की इच्छा करे, तब उसे केवल इतना ही करना है कि माँ के निकट भाग कर जाये और उन्हें स्पर्श कर ले। ऐसा करने से ही इस जगत्-क्रीड़ा के बन्धन से उसे सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसी से माँ के भक्तों ने इस जगत्-नाटक के विषय में बतलाते हुए इस खेल के सम्बन्ध में कितने मधुर व आन्तरिक भाव से बतलाया है कि इस खेल का आरम्भ माँ ही करती हैं और इसका अन्त भी वे ही करती हैं
रहस्यमयी माँ काली
देवी के विभिन्न रूपों के सम्बन्ध में विचार करते हुए हम एक विषम समस्या में पड़ जाते हैं। देवी-पूजा के प्रथम चरित्र के रूप के विषय पर विचार करने से सामान्य मानव का मन कुछ उद्घान्त हो जाता है। हमारे भाव, विचारधारा तथा संस्कृति से अनभिज्ञ विदेशियों की बात जाने दें, हमारे भारत के ही अनेक शिक्षित व बुद्धिमान् हिन्दू भी, जिसको अपनी माँ कह कर ध्यान करते हैं, उसी की इस सर्वसंहारकारिणी अत्युग्र विकराल मूर्ति की कल्पना का कारण समझने में असमर्थ हैं।
बंगाल प्रदेश में समस्त दशहरा पूजा ही माँ के इस दुर्गा तथा महाकाली के रूप की पूजा है। अनेक लोगों में काली का नाम मात्र भय उत्पन्न करता है। हिन्दू भी अपने मन में सोचते हैं कि काली के उपासक तामसी होते हैं। काली एक भयंकर व भीषण देवी हैं। मैं अपनी निजी अभिज्ञता के आधार पर कह सकता हूँ कि दक्षिण भारत में किसी रूढ़िवादी गृहस्थ के घर में यदि कृष्णवर्णा, रक्तवर्णा विस्तृत लोलजिह्वा, मुण्डमालाविभूषिता, छिन्नहस्तकटिपरिधानपरिवृता, रुधिरप्लुता खड्गधृतहस्ता काली की मूर्ति रखें, तो घर की स्त्रियाँ उसे तुरन्त ही बाहर निकलवा देंगी। यदि माँ काली के सम्बन्ध में उनकी यह धारणा उचित है, तो उनकी किस प्रकार मातृ-रूप में धारणा और पूजा की जाये?
यह भूल स्वाभाविक है और इसका संशोधन करना आवश्यक है। माँ कभी भी भीषण व भयंकर नहीं हो सकती हैं। वह सदा ही प्रेममयी और दयामयी हैं। महाशक्ति के अन्य सम्पूर्ण रूपों में माँ की काली के रूप में उपासना का अति-सहज कारण है। यह कोई दुर्बोध, गूढ़ आध्यात्मिक अथवा कोई गम्भीर दार्शनिक तत्त्वपूर्ण नहीं है, यह अत्यन्त सहज व अत्यन्त स्वाभाविक है।
मैं एक आधुनिक अद्यतन उदाहरण देता हूँ, जिससे यह विषय सहज ही बोधगम्य हो जायेगा। वर्तमान काल में पेनसिलिन व विभिन्न माइसिन जाति की ऐण्टीबाइटिक्स का प्रचलन है। नूतन युग ने उसे जीवन रक्षक महौषधि नाम दे रखा है और उसके ऊपर लोगों की अगाध श्रद्धा व विश्वास है। मैं दिखलाता हूँ कि ये सम्पूर्ण औषधियाँ मनुष्य के लिए हितकारी तथा रोगनाशक होते हुए भी भीषण ध्वंसकारी वस्तु भी कही जा सकती हैं। वे तुम्हारे रोग के कीटाणुओं की भीषण ध्वंसकारी हैं और उनको समूल नष्ट करती हैं। तुम रोगाक्रान्त हो, तुम्हारा शरीर रोग के कीटाणुओं से परिपूर्ण है जो तुम्हें रुग्ण किये हुए हैं। तुम पेनसिलिन लेते हो और यह तुम्हारे रोग के कीटाणुओं को ध्वंस कर देता है। इस भाँति कीटाणुओं के ध्वंस व संहार के द्वारा तुम्हारा रोग दूर हो जाता है और तुम स्वस्थ हो जाते हो। तब तुम क्या इस जीवनदायी महौषधि को ध्वंसकारी कहना चाहोगे? यदि इन्हें भीषण और ध्वंसकारी कहा जा सकता है, तो माँ काली को भी भीषण और ध्वंसकारी कह सकते हैं, अन्यथा नहीं।
संरक्षण के लिए ही यह संहार
इस प्रकार माँ रक्षा के लिए ही संहार करती हैं। ज्ञान-दान के लिए वह अज्ञानता व मोह नष्ट करती हैं। हमारा अन्धकार नष्ट करती हैं जिससे कि हम प्रकाश प्राप्त करें। वह सम्पूर्ण सन्ताप, दुःख और सम्पूर्ण भौतिक आधि-व्याधि और उपाधि नष्ट कर हमें आनन्द, सुख व अमृतत्व प्रदान करती हैं। इस भाँति वह जो-कुछ भी जीव को इस भयानक संसार में आबद्ध करता है, उसे नष्ट कर डालती हैं। वह जो कुछ भी भयंकर है, उसे ध्वंस कर सुख तथा शान्ति लाती हैं। जिस प्रकार इच्छा-शक्ति से, जो कि मन का ही एक अंश है, उसी मन में अवस्थित दुर्बलता व नीचता को दूर करते हैं, उसी प्रकार माँ निज संहार-शक्ति रूप से अपने ही एक दूसरे अंश का नाश करती हैं। माँ विद्यामाया रूप में अपने काली रूप द्वारा अविद्या नष्ट कर ब्रह्म के साथ योग कराती हैं।
इस भाँति हम देखते हैं कि महिमामयी माँ काली मोह से हमारा उद्धार करती हैं। उसके भक्त जन इसी भाव से माँ की काली रूप में पूजा करते हैं। वे माँ से कहते हैं-"हे दयामयी माँ! मैं अति-प्रबल मन के अधीन हो चला हूँ। अहंकार व इन्द्रियों द्वारा मैं पीड़ित हूँ। षड्रिपुओं, असंख्य वासनाओं, प्रवृत्तियों और संस्कारों का दास बन गया हूँ। वे सदा मेरे विरुद्ध युद्धरत हैं। एकमात्र तुम्हीं इन प्रबल शत्रुओं के हाथ से मेरी रक्षा कर सकती हो।" जब वे स्वयं उनके साथ युद्ध करने व उन्हें पराजित करने में असमर्थ होते हैं, तब वे माँ के शरणापन्न होते हैं और माँ की शक्ति की सहायता चाहते हैं। माँ कृपा करके उन्हें अपनी शक्ति देती हैं और उस समय माँ इस काली रूप विकराल मूर्ति में आ कर उन्हें अपनी इन्द्रियों को पराभूत करने तथा मन को स्व-वश में ला कर उस पर विजय प्राप्त करने में उनकी सहायता करती हैं।
नवरात्र में जिस दुर्गासप्तशती का पाठ किया जाता है, उसका विषय यही है। इसमें कुल तेरह अध्याय हैं। किस रूप से देवी-देवताओं के पक्ष में युद्ध में अवतीर्ण हो कर जो-कुछ अज्ञानता, पापाचार तथा परम सत्य के विपरीत है, उसे ध्वंस कर देती हैं-यह सब उसमें बतलाया है। इसमें असत्य के विभिन्न रूपों की विभिन्न दैत्यों के रूप में कल्पना की गयी है। अज्ञान के विभिन्न स्तरों को विभिन्न दैत्य कह कर उनके स्वभावानुसार उन्हें विभिन्न नाम व रूप दिया गया है। इन तेरह अध्यायों में माँ विभिन्न रूप धारण कर सब प्रकार के दोष, अज्ञानता व जगद्व्यापी माया को सर्वभावेन ध्वंस कर देती हैं, इस विषय का वर्णन किया गया है और अन्त में ज्ञान व विद्या-शक्ति की सम्पूर्ण भाव से जय और जीव की अज्ञान के हाथों में चिरमुक्ति प्रदर्शित की गयी है।
इस प्रकार की कल्पना मात्र हमारे देश की देवी-उपासना तथा शाक्त-सम्प्रदाय में ही आबद्ध नहीं है। संसार के सभी धर्मों में इस प्रकार के रूपक का व्यवहार पाया जाता है। ईसाई धर्मग्रन्थ में भगवान् तथा शैतान की कथा है। जो कुछ भी दैवी है, आलोकपूर्ण है-उसका विरोधी ही शैतान है। पारसी धर्मशास्त्र में अरमान तथा अहुरमज़दा है। अरमान ईसाई धर्म के शैतान का पर्यायवाची है। बौद्ध ग्रन्थ में मार की कथा है। उसी प्रकार हिन्दू-शास्त्र में जो कुछ दुष्ट तथा पापपूर्ण है, उसे माया, अज्ञान अथवा आसुरी शक्ति कहा गया है। यह प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञान तथा आत्मा का विपरीत धर्मी है। वेदान्त में उसे आत्मज्ञान द्वारा विदूरणीय अनात्मा कहते हैं। सप्तशती की यही मूल विषय-वस्तु है। इसमें माँ अपने काली-रूप में अपनी सन्तान की उसके दुर्गुणों के नाश करने में सहायता करती हैं।
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ।
दारिद्र्यदु:खभयहारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्रचित्ता ।।
(दुर्गासप्तशती : ४-१७)
माँ दुर्गे ! स्मरण मात्र से सब जीवों का त्रास हरे।
स्वस्थ जनों द्वारा चिन्तन से, शुभ सम्मति प्रदान करे ।
दुःखदरिद्रभयहर्ता देवी आप बिना को अन्य करे।
पर उपकारीवश दवाई हो सब जीवों पर कृपा करे ।।
तृतीय रात्रि
ॐ दुं दुर्गायै नम
ध्वंस ही सृष्टि का मूल
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः I।
(दुर्गासप्तशती : ५-५२)
जो देवी श्रद्धास्वरूप से व्याप्त सर्वभूतों में माँ।
नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है उसे नमः ।।
सारे साधकों की चरम गति व लक्ष्य माँ ही हैं। परब्रह्म व परम माँ एक हैं। जो जगत् की सृष्टि, स्थिति व संहारकारिणी हैं, उन्हें बार-बार प्रणाम !
कल हमने माँ के दुर्गा व भीषण काली-रूप की चर्चा की थी और यह देखने तथा जानने की चेष्टा की थी कि बाहर से कराल-मूर्ति व प्रत्यक्षतः ध्वंस की लीला के अन्दर माँ वस्तुतः कैसे कल्याणमयी व दयामयी रूप में रहती हैं। उनका ध्वंस सृष्टि के लिए ही, उनका आहरण प्रचुर प्रदान के लिए ही होता है। वह अन्त में अज्ञान के गहन अन्धकार को ध्वंस करने में हमारी सहायता कर अपने को ज्योतियों की ज्योति, आत्मा के शाश्वत प्रकाश के रूप में हमारे समक्ष प्रकट करती हैं।
माँ दुर्गा की इस भीषण संहार-मूर्ति के आविर्भाव की कथा ही वास्तव में हमारे अनुसन्धान का विषय है। सप्तशती के एक श्लोक में दुर्गा-नाम की व्याख्या में बतलाया है कि जो सम्पूर्ण दुर्गति का हरण करती हैं, जो सम्पूर्ण प्रकार के विपद् व दुःख से रक्षा करती हैं, वही दुर्गा हैं। वह अपने भक्तों के सम्पूर्ण कष्ट, अमंगल व सम्पूर्ण आर्ति हर लेती हैं। इसीलिए वह दुर्गा देवी के नाम से अभिहित हैं। यह केवल आध्यात्मिक व्याख्या की ही वस्तु नहीं है, यह व्यापक अनुभव पर आधारित सत्य है कि यह सर्वसंहारिणी शक्ति सम्पूर्ण अमंगल व सम्पूर्ण अशुभ को ध्वंस करने में सक्षम हैं।
जीवन के मध्य में ही ध्वंस की क्रीड़ा रहती है
हम देखते हैं कि इस जगत् में और मानव-जीवन में ध्वंस-कार्य सदा ही चलता रहता है। ध्वंस के बिना जीवन की गति सम्भव नहीं है। धारावाहिक सृष्टि-कार्य में ध्वंस एक अंग है। मनुष्य के दैनन्दिन जीवन की आलोचना करने पर यह सहज ही उपलब्ध होता है। 'अन्नगताः प्राणाः' मनुष्य के स्थूल शरीर के सम्बन्ध में कहा। गया है। अन्न 1 बन्द कर देने पर शरीर भी नष्ट हो जाता है। आइए, अब हम शरीर-पोषण तथा जीवन-रक्षा की प्रक्रिया पर विचार करें। आहार-उत्पादन कार्य ही अनेक प्रकार के ध्वंस-कार्यों द्वारा सम्पन्न होता है। शस्य के उत्पादन के लिए भूमि के ऊपर से प्रथम झाड़-झंखाड़ और जंगली पौधों का ध्वंस करना होता है। तत्पश्चात् भूमि का कर्षण करना होता है। विशेष उपकरणों से भूमि को खोदना होता है। इससे धरती आहत होती है। तदुपरान्त ही बीज वपन किया जाता है। यह बीज शस्य-रूप में अंकुरित होने के लिए अपना जीवन देता है। अन्न के उत्पन्न होने तक विनाश की यह प्रक्रिया सतत चालू रहती है। तत्पश्चात् भूसी निकालनी होती है। तब अन्न प्राप्त होता है। छिलके के विनाश से ही अन्न उपलब्ध हो पाता है। इस अन्न का भोजन बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कुल्हाड़ी के क्रूर आघात से वृक्षों का विनाश करना पड़ता है। इस काष्ठ को भी अग्नि की ज्वाला में आत्म-दाह करना पड़ता है। इस भाँति अपना विनाश कर वह ताप देता है, तब आहार बनता है। भोजन करने वाले मेज के सामने बैठ कर इस पके हुए भोजन को खा कर नष्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अन्न का आकार, प्रकार तथा स्वरूप विनष्ट होता है। इस भाँति अन्न के मनुष्य के शरीर में पहुँच कर जीवन-शक्ति में रूपान्तरित होने तक विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है। यह तो केवल एक प्रारूपिक उदाहरण है। इसी भाँति यदि हम मानव जीवन के किसी भी भाग को देखें, तो हम पायेंगे कि जगत् में जो कुछ निर्माण होता है, उसका आधार विनाश-परम्परा ही होती है। अन्त में इन सबका परिणाम आकांक्षित नव-रचना के रूप में ही मिलता है।
बृहत्तर रूप में भी हम देखते हैं कि जगत् में जीव-सृष्टि के निर्वाह के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है। यदि मृत्यु द्वारा मानव शरीर का विनाश न होता रहता, तो अर्थशास्त्री माल्थस के सिद्धान्त के अनुसार इस अधिक जनसंख्या-आकीर्ण पृथ्वी पर लोगों को खाने के लिए अन्न तथा रहने के लिए स्थान उपलब्ध न हो पाता। अधिक जनसंख्या सामान्य मनुष्य को दृष्टिगोचर न होने के कारण उनके लिए भयावह पिशाच नहीं है, किन्तु व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले अर्थशास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों को अधिक जनसंख्या मानव-जाति के लिए एक शाश्वत अभिशाप है। माता का यह विनाशकारी रूप इस प्रकार मानव-शरीर की मृत्यु तथा विलय की गति द्वारा अधिक जनसंख्या के भूत को दूर रखता है और मानव जाति की रक्षा करता है। ऐसा होते हुए भी, जनसंख्या बढ़ती ही जाती है और जब वह जीवन की आवश्यकताओं के उत्पादन की क्षमता से भी कहीं अधिक हो जाती है और जब मनुष्य के सम्मुख ऐसी स्थिति आ उपस्थित होती है, तो वह काँप उठता है और जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि अर्थशास्त्री और राजनैतिक पुरुष भी आकुल हो उठते हैं, तब ही करुणामयी व स्नेहमयी माँ की संहारक शक्ति सहायतार्थ दौड़ कर आ जाती है। अधिक जनसंख्या के विकराल राक्षस को किस प्रकार रोका जाये, यह मनुष्य नहीं जान पाता, तब माता ही भूकम्प, युद्ध, दूर-विस्तृत दुष्काल, जल-बाढ़ तथा महामारी के रूप में प्रकट हो कर परिस्थिति को उग्र रूप धारण करने से रोक देती हैं।
यदि हम मानव-जीवन की समस्त प्रक्रियाओं में से प्रत्येक पर पृथक् पृथक् रूप से विचार करें, तो पायेंगे कि अतीव रचनात्मक प्रक्रिया भी आवश्यक तथा अपरिहार्य है और मनुष्य की मानी हुई संहारक प्रक्रिया का पराकाष्ठा रूप ही है। साधारण मनुष्य के लिए ध्वंस का अर्थ है अस्तित्व का लोप। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन संहारकारिणी दुर्गा व काली के दार्शनिक तत्त्वज्ञान का आधार है। यह दर्शन है एक ध्वंस ला कर क्रमोन्नयन-निम्न अवस्था से, स्थूल अवस्था से उच्च व सूक्ष्म अवस्था की ओर गमन। अन्धकार का नाश ही आलोक का धर्म है। अन्धकार का नाश हुए बिना प्रकाश का आगमन नहीं हो सकता है। अपवित्रता का अतिक्रमण किये बिना पवित्रता नहीं आ सकती है। इसी भाँति छोटे का ध्वंस होने पर ही बड़े का आविर्भाव होता है।
ध्वंस नहीं ऊर्धीकरण
आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्वंस का अर्थ है उन्नयन, निम्न अवस्था से उच्चतर अवस्था की ओर गमन। जहाँ-कहीं भी विकास की विधान-परम्परा की योजना की गयी है, वहाँ पर प्रत्येक अल्प एवं निम्न स्वरूप के विनाश की परम्परा भी संयोजित हुई दीख पड़ती है। यह अल्प और निम्न स्वरूप अपने से उच्चतर स्वरूप को अपना स्थान देते और स्वयं विनाश को प्राप्त होते हैं। अतः यह ध्वंस हमारे लिए आवश्यक है। ऊपर की दिशा में जाने के लिए यह प्रयोजनीय है। इससे भय करके इससे बचने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम अशुद्ध वस्तुओं से चिपके रहते हैं, जब तक हम अशुद्धियों का त्याग नहीं करते, तब तक उन्नति करना शक्य न होगा। दिव्य शक्ति के हस्तक्षेप द्वारा निम्नता के नाश होने के पश्चात् ही उच्चता की प्राप्ति सम्भव हो पाती है। योग तथा साधना की विशिष्ट प्रक्रिया में माता जी के दुर्गा अथवा परम कृपालु काली माता का स्वरूप क्या भाग अदा करता है, इस पर आज हम विशेष रूप से विचार करेंगे। हम यह देखेंगे कि साधक को अपने जीवन में किस भाव से माँ की आराधना करनी होती है. किस भाव से अन्तर में माँ का रूप उद्घाटित होता है एवं किस भाव से वह साधक को उसके योग-साधना के पथ में सहायता व साफल्य प्रदान करती हैं। किन्तु इन सब पर विचार करने से पूर्व योग-साधना की प्रक्रिया के विषय में विचार कर लेना ठीक होगा।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग-साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने स्वभाव की अपूर्णताओं, संकीर्णताओं, मानवीय दोषों, दुर्बलताओं तथा हीनताओं को पार कर अनन्त एवं शाश्वत दिव्य चेतना का अनुभव करने को उन्नत होता है। आध्यात्मिक जीवन तथा योग-साधना द्वारा इस कार्य को आरम्भ करने में साधक को एक विचित्र परिस्थिति का, एक समस्या का सामना करना पड़ता है। एक डग में ही मानव-स्वभाव से दैवी स्वरूप तक पहुँच जायेंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है। जब साधक इस कार्य के लिए आगे पग रखना आरम्भ करता है, तब उसे ज्ञात होता है कि मनुष्य-प्रकृति में मनुष्य-जीवन से नीचे के अनेक धर्म अन्तर्निहित है। हिन्दू-संस्कृति में इसका वर्णन एक विशेष ढंग से किया गया है जो कि इसकी अपनी विशिष्टता है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त में ऐसा बताया गया है कि मानव-देह प्राप्त करने तक जीव अविकसित खनिज पदार्थों, वनस्पतियों तथा एक कोषाणु वाले जीव जैसी निम्न श्रेणी की असंख्य योनियों से हो कर गुजरता है। इन निम्न कोटि की असंख्य योनियों से गुजरते समय उसकी चेतना प्रत्येक जन्म के प्रधान गुणों के संस्कार ग्रहण करती है। इस कारण मनुष्य-देह लाभ करने पर भी वह मानव सहज बुद्धि, विवेक तथा विचार-शक्ति के साथ-ही-साथ मानवेतर योनि के अनेक पूर्व-प्राप्त संस्कारों व प्रवृत्तियों को वहन कर लाया है। इसीलिए अनेक बार कितने ही मनुष्यों में ऐसे गुण देखने को मिलते हैं जो सामान्य रूप से पशुओं में ही पाये जाते हैं यथा लोमड़ी की धूर्तता, व्याघ्र की नृशंसता, वृश्चिक की विषाक्तता, क्षुद्र जीवों की प्रमाद-वृत्ति, शूकर का पेटूपन तथा मानवता की श्रेणी में न आने वाले अन्य सभी दुर्गुण। पशु-योनि से ऊर्ध्व गति पा लेने पर भी ये संस्कार उसके स्वभाव में वर्तमान रहते हैं। अतः ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य वस्तुतः पशु ही है। हाँ, अन्तर केवल इतना है कि वह विवेक, ज्ञान तथा विचार-शक्ति से सम्पन्न है। इस भाँति मानव-प्राणी एक त्रिक है। वह दैवीभावापन्न मनुष्य और पशुभावापन्न मनुष्य के मध्य की अवस्था में रह रहा है। उसके एक ओर पाशविक स्वभाव है और दूसरी ओर दैवी स्वभाव है। इसी से कभी-कभी वह प्रमाद, काम, क्रोध, हिंसा प्रभृति पाशवी वृत्तियों से नीचे की ओर खिंचता है, तो कभी-कभी विरल क्षणों में उत्कृष्ट उन्नत अवस्था को प्राप्त कर करुणा, न्याय, सत्यता, पवित्रता प्रभृति दिव्य गुणों को प्रकट करता है। इस भाँति वह दो भावों से दोलायमान रहता है।
अपने अन्दर के पशु-भाव की बलि दो
साधक का प्रथम और प्रधान कर्तव्य है अपनी निम्न प्रकृति के, आसुरी प्रकृति के भावों का समूल उत्पाटन। इस प्रकार के भावों को पूर्ण रूप से सुसंस्कृत करना होगा और अपने स्वभाव से इनका उन्मूलन करना होगा। इसके अनन्तर दैवी भाव में उन्नयन का कार्य हाथ में लेना होगा। मानवी भाव से उत्कर्ष द्वारा दैवी भाव में, उच्च स्तर के दैवी भाव में ले जाना होगा। मनुष्य एक संग्रथित प्राणी है। वह निम्न पाशवी तत्त्वों से, सारासार की विचार-शक्ति से, उच्चतर आदर्शों की चेतना के इस पार्थिव जगत् में मानव-योनि में जन्म लेने के भव्य दिव्य उद्देश्य की चेतना से तथा दिव्य उच्चतर आदशों तक उन्नत होने की क्षमता के तत्त्वों से समन्वित है। मनुष्य के अन्दर जो पशुत्व भाव है, उन्हें उच्च मानवोचित भाव में ले जाने के विषय में चिन्तन करते-करते मनुष्य पशु-बलि अथच नर-बलि के चिन्तन पर जा पहुँचा। माँ के मन्दिर में, माँ के पदतल के नीचे पशु-भाव की बलि से पशु-बलि की प्रथा का प्रचलन हुआ। प्रथम जहाँ मन के पशु-भाव को माँ के श्रीचरणों में निवेदन कर मन को पवित्र करने का विचार था, वहीं काल-क्रम से पशु-भाव के प्रतीक-रूप वास्तविक जीवित पशु को माँ की वेदी के मूल पर बलि दिया जाने लगा। मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की आन्तरिक प्रक्रिया की एक आदर्श भावना अधोगति को प्राप्त हो बाह्य प्रथा बन गयी। साधक के साधना-जीवन की प्रथम अवस्था में उसके जो नीच, पशु-भाव हैं, उन्हें माँ दुर्गा अथवा श्री काली के चरणों में निवेदन करना तथा उनकी कृपा व शक्ति द्वारा उसके चिरकालजन्य पशु-भाव को पूर्णतया ध्वंस कर साधना-राज्य में अग्रसर होना ही इस बलि-प्रथा का अन्तर्निहित तत्त्व है।
इस उद्देश्य के लिए साधक को प्रथम अपने मन का गम्भीर विश्लेषण करके यह निश्चय करना होगा कि कौन-सा पशु-भाव उसके व्यक्तित्व में तीव्र रूप से वर्तमान है। कोई व्यक्ति अन्य विकारों की अपेक्षा क्रोध का, कोई विषय-वासना का तो कोई किसी अन्य विकार का दास होता है। किसी-किसी को ऐसा भी लगता है कि भिन्न-भिन्न विकारों तथा वासनाओं का उसके व्यक्तित्व के ऊपर अधिकार है और वे उसे दास बनाये हुए हैं। ऐसा भी होता है कि कभी एक तो कभी कोई दूसरा विकार अपना प्रभुत्व जमाता है। अतः प्रथम कार्य है आत्म-निरीक्षण करना, आत्म-विश्लेषण करना तथा पता लगाना कि उसके स्वभाव में कौन-सा दुर्गुण कार्य कर रहा है। अतः अपने मन का प्रामाणिक अध्ययन साधक के लिए नितान्त अपरिहार्य कर्तव्य है। उसको जब तक यह ज्ञान न हो कि उसके मन के भीतर कौन-सा तत्त्व है जो योग में सफलता के लिए अवांछनीय है, शत्रु है, जो साधना में अवरोध करता है, तब तक इस आन्तरिक तथा दुर्गम योग-पथ पर ठीक से अग्रसर होना सम्भव न होगा। यह कार्य इसलिए दुस्साध्य है कि ये सब तमोगुण, मनुष्य स्वभाव के नीच भाव साधारणतः स्पष्ट रूप से बाहर कम ही प्रकट होते हैं।
बाहर के शत्रुओं का सामना करना सरल है, क्योंकि हम उन्हें, उनके स्वभाव तथा सामर्थ्य को जान सकते हैं और इसलिए उनके समरूप ही उनका सामना कर सकते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा प्रभृति मनुष्य के अन्दर के शत्रु नाना रूप धारण करते हैं और वे हमारी दृष्टि से अगोचर ही रहते हैं। वे विविध छद्मवेश में छिपे रहते हैं। अतः यदि साधक प्रार्थना द्वारा अन्तर्यामी की, अपने हृदय में अवस्थित परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता तो अपने इस नीच स्वार्थपूर्ण, अहंकारपूर्ण स्वभाव को नष्ट करने के कार्य में प्रगति नहीं कर सकता। किसी दूसरे व्यक्ति के सम्बन्ध में विचार करना सरल है; क्योंकि उसका बाह्याचरण हमारे दृष्टि-पथ के अन्दर है, किन्तु अपने अन्तर का विचार करना अतीव दुरुह कार्य है। इसका कारण यह है कि मानव-मन स्वभावतः बहिर्मुखी है। यह बाहर के जागतिक पदार्थों की ओर सदा भागा फिरता है। प्रथम उसे अन्तर्मुखी करना दुस्साध्य है। विपरीत दिशा में ले जाना बहुत ही कष्टकर होता है। द्वितीयत, मनुष्य का अहंकार अपने दोषों को, अपनी त्रुटियों को देखने या खोजने नहीं देता। जिस वस्तु से अपने अहं को पोषण नहीं मिलता, उसे देखने तथा जानने को मन तैयार नहीं होता। साधारणतया यह देखा गया है कि जो हमारे अहंकार के लिए सुखप्रद नहीं है, वह सदा ही हमारी दृष्टि से बाहर रहता है।
अपना विश्लेषण स्वयं करने में अतीव दुरूह है। इसीलिए पौर्वात्य आध्यात्मिक साधना-मार्ग में साधक को सद्गुरु की शरण लेने को कहा जाता है। वह सद्गुरु के निकट जा कर, उनको सम्पूर्ण भाव से आत्म-समर्पण कर उनके सान्निध्य में निवास करता है। ऐसा होने पर उसके वे सम्पूर्ण दोष जिन्हें वह अपनी चेष्टा से देख नहीं सकता अथवा अपने विश्लेषण से पकड़ नहीं पाता, गुरु के नेत्रों से सहज ही पकड़ में आ जाते हैं। तब सद्गुरु उसको इस रूप में चलाते हैं जिससे कि वह सहज ही उन सब दोषों पर विजय पा लेता है, किंवा उसे इस प्रकार का कार्य करने का आदेश देते हैं जिसमें इस प्रकार के दुर्गुणों का उन्मूलन नितान्त अपरिहार्य हो जाता है। कभी-कभी वे उसे उपदेश देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसकी भर्त्सना भी करते हैं। साधक की दृष्टि की पकड़ में जो दोष नहीं आते, वे सद्गुरु की दृष्टि से अगोचर नहीं रह सकते। इससे उनको नष्ट करना सरल हो जाता है। इस भाँति, गुरु भी एक बड़ी सीमा तक काली माता का भाग अदा करता है और साधक की दुर्वृत्तियों तथा दुर्गुणों को नष्ट कर अध्यात्म-मार्ग में अवरोध करने वाले अन्तरायों को ध्वंस कर देता है।
आध्यात्मिक साधना में दुर्गा का प्राकट्य
माँ दुर्गा गुरु की मूर्ति में और गुरु के भीतर अपने को प्रकट करती हैं। शिष्य के मन में ऊर्ध्वमुखी गति की तीव्र आकांक्षा के रूप में माँ का ही प्रकाश है और कठोर आत्म-परीक्षण तथा आत्म-निरीक्षण के रूप में माँ का ही विकास है। जब इस प्रकार के आत्म-निरीक्षण से साधक के अन्तःचक्षु के सामने उसके पशु-भाव का चित्र पूर्ण विवरण के साथ प्रकट हो, तब माँ की आराधना कर इन सब पशु-भावों के ध्वंसार्थ तीव्र व दृढ़ भाव से प्रार्थना करनी होती है। उस समय, माँ की इस भीषण ध्वंसमयी मूर्ति के ध्यान तथा आराधना की आवश्यकता होती है। योग के पथ में प्रथम पग पर ही माँ की इस सर्व-अशुभ-वृत्ति की संहारिणी-शक्ति के निकट प्रार्थना करनी होती है, जिससे कि हमारे योग-पथ की सब बाधाएँ दूर हो जायें और हम अग्रसर हो सकें। अपने दोषों के विषय की अज्ञानता इस पथ का प्रथम अन्तराय है। इस अन्तराय को पार कर लेना और अपने दोषों को जान लेना मात्र ही हमारे लिए पर्याप्त न होगा। अपने दोषों को जान लेने पर भी यदि हम उन्हें दूर करने के लिए कुछ न करें, तो वे दोष चिरकाल तक बने रहेंगे और हम प्रगति नहीं कर सकेंगे। उसके पश्चात् का आगामी पग है और अपने अन्दर की अधोगामी वृत्तियों को समूल नष्ट करने का दृढ़ संकल्प व प्रबल इच्छा-शक्ति को जाग्रत करना। जब एक बार इस प्रबल इच्छा-शक्ति की आराधना की जाती है, तो पशु-भाव को विजित कर उस पर आधिपत्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा-शक्ति व दृढ़ संकल्प के रूप में माँ स्वयं ही साधक के अन्दर प्रकट होती हैं।
इसके पश्चात् माता जी कर्ममयी इच्छा-शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। इस इच्छा-शक्ति को क्रिया-शक्ति तथा साधक में साधना-शक्ति में परिणत करना होता है। इस शक्ति के बल से ही साधक अपने दैनन्दिन जीवन के सभी क्षणों में, अपने सम्पूर्ण कार्यों में, दूसरों के साथ व्यवहार में, अपने विचार, उद्देश्य तथा भाव में अपनी सम्पूर्ण दुष्ट वृत्तियों का सामना करना आरम्भ कर देता है। यह कार्य साधना-शक्ति-रूपा भगवती माँ के कारण ही शक्य हो पाता है। इस भाव से साधना चालू रहनी चाहिए। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए साधना-शक्ति रूप में दिव्य माता का आविर्भाव करना तथा अपनी सम्पूर्ण प्रकार की यौगिक प्रचेष्टाओं को प्रयोग में लाना होगा। इस समय यदि साधक को निम्नगामी वासना आकर्षित करती है तो उसे तपश्चर्या, उन बस्तुओं के त्याग, उन वासनाओं के निरोध जैसी साधना-प्रक्रियाओं का आश्रय ले कर उन वासनाओं को पूर्णतया नष्ट करना होगा।
ऐसा कहा जाता है कि वासनाओं को तुष्ट न करने पर वे व्यक्ति के मन में गुप्त रूप से निवास करती हैं और उपयुक्त अवसर आने पर नाना प्रकार के प्रलोभनों के रूप में प्रकट हो कर उस पर विजय प्राप्त करती हैं। यहाँ पर हम एक महान् सत्य प्रस्तुत करते हैं। ऐसा पाया गया है कि वासनाओं की पूर्ति द्वारा उन पर विजय प्राप्त करना इस लोक में सर्वाधिक दुस्साध्य कार्य है। वासना प्रज्वलित अग्नि के समान है। वासनाओं को तुष्ट करने का प्रयास घृणाहुति डालने का कार्य करता है। अग्नि में आहुति डालने से हम वस्तुतः उसे जलाने को कुछ देते हैं और उसको जलाने से वह और अधिक प्रचण्डता से, और अधिक भीषणता से प्रज्वलित हो उठती है। इसके विपरीत, दाह्य वस्तु के अभाव में अग्नि का स्वाभाविक ही नाश हो जाता है। इसी प्रकार इन्द्रिय की परितृप्ति के विषय का अभाव होने पर इन्द्रिय की तृष्णा स्वयमेव नष्ट हो जाती है। इस प्रकार दुर्गा माता तपश्चर्या के रूप में साधक में व्यक्त होती हैं।
तपश्चर्या का कष्ट सहन करने के लिए तितिक्षा-शक्ति की वृद्धि करनी होती है। मन को अति-अरुचिकर स्थिति को सहन करने की शक्ति को, मानव के निम्न प्रकृति के लिए असुखकर तथा अवांछनीय वस्तुओं को सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा के अनेक रूप व नियम हैं। उपवास, जागरण आदि तथा आत्म- त्याग अर्थात् मन के रुचिकर पदार्थों का कुछ काल के लिए त्याग यथा लवण-शून्य भोजन, शर्करा-रहित चाय, पादुका त्याग प्रभृति इसी श्रेणी में आते हैं।
प्रत्येक साधक को अपनी सहज अधोगामी वृत्तियों की रोक-थाम करने तथा विषय-जगत् की ओर व्यक्ति को आकर्षित करने वाली ऐन्द्रिक वासनाओं पर नियन्त्रण प्राप्त करने के उपायों पर बुद्धिपूर्वक विचार कर अपनी व्यक्तिगत साधना का सम्पूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। अपनी इन सब सम्मिलित चेष्टाओं के रूप में माता जी की भिन्न-भिन्न शक्तियों के आविर्भाव के परिणाम स्वरूप साधक आध्यात्मिक जीवन तथा साधना के प्रथम प्रक्रम का अतिक्रमण कर पाशवी वृत्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है।
इस भाँति पशु-बलि का कार्य माँ की पापनाशिनी, तमोहारिणी, अज्ञान- विनाशिनी दैवी शक्ति की उपासना द्वारा ही साधित हो सकता है। साधक के आध्यात्मिक जीवन में माँ काली की पूजा का यही उद्देश्य व अर्थ है।
साधक के जीवन में माँ दुर्गा की विभिन्न धाराओं के विकास पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालना किसी भी व्यक्ति के लिए असम्भव ही है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि इस पर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं विचार करे और अपने ध्येय में उसे प्रकट करने हेतु कार्य करे। इस विषय की सामान्य चर्चा करते हुए हम साधारण रूप से इतना ही कह सकते हैं कि कठोर आत्म-निरीक्षण, दृढ़ निश्चय तथा इस निश्चय को साकार रूप देने वाली कर्ममयी चेष्टा तथा तप, सहनशीलता, आत्म-संयम, उपवास प्रभृति योग-साधना के सहकारी उपाय के रूप में माँ को उनके विविध रूपों में अपने अन्तर में प्रकट करना होता है।
सप्तशती की शिक्षा
यदि हमें उच्चतर दिव्य चेतना को प्राप्त करना है, तो हमें मानव-स्वभाव और तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकार की भ्रान्त धारणाओं से ऊपर उठना है। साधक की मानवीय चेतना के ऊपर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया 'नर-बलि' का प्रतीक है।
सप्तशती तीन विभागों में विभक्त है। प्रथम विभाग में मधु-कैटभ का वध, द्वितीय विभाग में महिषासुर-मर्दन तथा तृतीय विभाग में अन्य असुरों के साथ शुम्भ-निशुम्भ भ्रातृ-द्वय के संहार की कथा है। ये तीनों विभाग साधना की तीन भूमिकाओं के प्रतीक हैं। मधु तथा कैटभ मनुष्य की निम्न प्रकृति के स्थूल रूप के प्रतीक हैं। महिषासुर-मर्दन इससे ऊपर की अवस्था अर्थात् रजोगुण के विनाश का प्रतीक है। जब हम तृतीय भाग में पहुँचते हैं, तो हम देखते हैं कि यह असुर कुछ उच्च कोटि का है। वह एक राजा है, बहुत ही धनवान् है, खूब शिक्षित है; किन्तु मिथ्या दम्भ-वृत्ति से परिवृत है। स्वर्गलोक पर उसका आधिपत्य है। भूलोक की समस्त सम्पत्ति का वह स्वामी है। सम्पूर्ण चतुर्दश भुवनों में जो भी काम्य पदार्थ हैं, सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं, उन पर इन दोनों अजेय भ्राताओं का अधिकार है। वे प्रभूत सैन्य के नेता हैं। उनके एक योद्धा का नाम रक्तबीज है। वह मनुष्य के अहं-भाव का प्रतीक है। इस अहं-भाव के ध्वंस होने पर ही शुम्भ-निशुम्भ का वध सम्भव हो पाता है। ये दोनों विक्षेप तथा आवरण-शक्ति के प्रतीक हैं। इनकी मृत्यु से मानव तथा दिव्य चैतन्य के बीच का अन्तिम अन्तराय भी जाता रहता है और माँ की कृपा से आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा पर पहुँच कर व्यक्ति परब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है।
भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा-
मिति स्तोतुं वांछन् कथयति भवानि त्वमिति यः ।
तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं
मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदाम् ।।'
(सौन्दर्यलहरी २२)
देवि! दास तुम्हारा मुझ पर करुण दृष्टि प्रसार करें।
'मातु भवानी। कहते ही स्तुतिकर्ता पर कृपा करें।।
और उसे देती निज पदवी जो सायुज्यमयी स्यन्दन।
ब्रह्मा विष्णु इन्द्र मुकुटों को झुका करें तव पद बन्दन ।।
चतुर्थ रात्रि
ॐ श्रीं ॐ
लक्ष्मी : परम पालयित्री
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ।।
(दुर्गासप्तशती : ११-१०)
मंगलमयी सब मंगलदाता, सर्व पुरुषार्थ साधिती माँ।
नारायणी गौरी त्र्यम्बके नमस्कार है तुम्हें नमः ।।
सबकी उत्पत्ति व लक्ष्यरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वशक्तिमान् परमात्मा की पराशक्तिरूपिणी माँ सरस्वती तुम्हें नमस्कार! महालक्ष्मीरूपिणी शक्ति तथा दुर्गारूपा आदि शक्ति तुम्हें नमस्कार !
आज सृष्टिकारिणी माँ-रूप में भावित भगवान् की पूजा का चतुर्थ दिवस है। आज हम इस गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण पूजा की द्वितीय भूमिका में प्रवेश करते हैं। आज से पराशक्ति की उनके एक नवीन रूप में, धारण व पोषणकारिणी माँ के रूप में आराधना आरम्भ होती है। आज से तीन दिन तक सारे भारत में माँ की महालक्ष्मी के रूप में पूजा की जायेगी। शेष तीन दिन माँ की महासरस्वती के रूप में पूजा कर दशम दिन विजयादशमी को इस पूजा की परिसमाप्ति होगी।
सूक्ष्म तथा स्थूल में अवतरण
नवरात्र-पूजा की इस विशिष्ट योजना पर विचार करते समय माँ भगवती के विविध रूपों की, क्रमशः दुर्गा, लक्ष्मी तथा सरस्वती की पूजा में एक गम्भीर सत्य का विकास दिखायी पड़ता है। यह स्वयं में एक स्वाभाविक नियम का ही प्रकाश है। अदृश्य तथा नाम और रूप से परे की परम शक्ति दृश्यमान् जगत् के रूप में दृष्टिगोचर बनती है तथा नाम और रूप धारण करती है। तब प्रतिगामी प्रक्रिया आरम्भ होती है, जो निरपेक्ष है वह सापेक्ष बनता है, जो अनामी है वह नाम धारण करता है, जो अरूप है वह रूपवान् बनता है। इस प्रक्रिया में सर्वोत्कृष्ट तत्त्व, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तत्त्व, आदि कारण व स्रोत क्रमशः स्थूल की ओर अग्रसर होता हुआ अन्त में जड़ पदार्थ में परिणत हो जाता है। यह प्रतिगामी प्रक्रिया प्रपंच के विकास का एक क्रम है। यह एक से अनेक बनने का, अव्यक्त से व्यक्त बनने का, कारण से विविध परिणाम-रूप में प्रकट होने का क्रम है। इसी भाँति जब साधक इस स्थूलोन्मुखी गति से अपनी मूल उत्कृष्ट स्थिति में पहुँचने का, ऊर्ध्वगामी होने का प्रयत्न करता है, भौतिक क्षेत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर अग्रसर होने की चेष्टा करता है, तो उसे अपने अन्दर की गति को पूर्व-गति के विपरीत दिशा में चलाना होता है। उस समय दिव्य शक्ति ठीक विपरीत दिशा में कार्य करना आरम्भ कर देती है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होना आरम्भ हो जाता है।
जब विकास-क्रिया आरम्भ होती है, तो प्रथम ब्रह्मा की सृजन-शक्ति काम करना आरम्भ कर देती है। सृजन-शक्ति की क्रिया-शक्ति के क्रियाशील होते ही पराप्रकृति से नामरूपात्मक सृष्टि की धारा प्रकट होती है। अव्याकृत से ये नाम और रूप माया के राज्य में प्रवेश करते हैं। उस समय ये भूत, वर्तमान और भविष्य नामक काल के आधिपत्य के नीचे आते हैं। उन्हें अपने नाम और रूप को प्रतिधारण करना और त्रिकाल में अपना अस्तित्व बनाये रखना होता है, इससे परिरक्षण, पालन, पोषण और रक्षण-शक्ति का कार्य आरम्भ हो जाता है। विश्व-प्रपंच के संचालक तथा जगत् के पालनकर्ता विष्णु की क्रिया-शक्ति के रूप में महाशक्ति कार्य करती हैं। वही महालक्ष्मी हैं। काल-प्रवाह की चपेट में आने से नाम और रूप परिवर्तनशील व क्षयिष्णु हैं। अतः उनमें परिवर्तन अनिवार्य है। नाम तथा रूप का विवर्तन तथा नाश की क्रिया जिसका कार्य है, वही रुद्र हैं। वह लय और ध्वंस के अधीश्वर हैं। इस प्रकार उत्पत्ति से विलय तक यह क्रिया चलती रहती है। यही स्थूल में अवतरण है।
मनुष्य की ईश्वरत्व-प्राप्ति
गीता में कहा है कि योगी जनों का कार्य साधारण जागतिक लोगों के कार्य से सर्वथा विपरीत हुआ करता है। सांसारिक मनुष्य का दिवस संयतात्मा के लिए रात्रि है। सांसारिक मनुष्य जिन बातों में जागृत है, उन बातों में योगी सोया रहता है और उनकी ओर कुछ ध्यान नहीं देता। अध्यात्म-जगत् में रहने वाली उन्नत भावनाओं में संसारी जीव सोया-सा रहता है, जब कि योगी इनमें पूर्ण जाग्रत रहता है। सांसारिक मनुष्य जिसे देखता है, उस ओर से योगी मुख फेर लेता है और सांसारिक मनुष्य जिस वस्तु को नहीं देख पाता, उसे योगी अपने आध्यात्मिक अवबोध की अवस्था में देखता है। इस नियम के अनुसार जब यह दिव्य शक्ति अन्तर चेतना के साम्राज्य में विकास की ऊर्ध्व प्रक्रिया आरम्भ करती है, तब साधक शक्ति की आराधना उलटी रीति से करता है; क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया अवतरण प्रक्रिया के विपरीत होती है।
सर्वप्रथम, साधक माता जी के संहारक रूप की उपासना करता है, जिससे जीव के ऊपर छायी हुई भौतिकता का नाश हो। जीवात्मा स्थूलता में, भौतिकता में अवतरित है, वह अज्ञान में निमग्न है। अतः जड़ की पकड़ से मुक्ति, अज्ञान तथा मोह-पाश का ध्वंस, अशुद्ध मूल तत्त्वों पर विजय तथा विशुद्ध, सूक्ष्म व आध्यात्मिक राज्य तक ऊर्ध्व गति प्रथम प्रक्रिया है। प्रथम जीव के स्थूल भाव तथा भौतिक जगत् के प्रभाव को नाश करने के लिए माता जी की शक्ति तथा बल-रूप में प्रार्थना की जाती है। इसके उपरान्त योग के पथ व आध्यात्मिक जीवन में उन्नीत हो कर साधक लक्ष्मी-रूपा माँ की आराधना करता है जिससे आध्यात्मिक जीवन में टिके रहने में जो कुछ भी आवश्यक है, वह सब उसे प्रदान करें।
व्यावहारिक जगत् में भी योग-क्षेम के वहन करने के लिए भी लक्ष्मी माता की आराधना आवश्यक है। यह सदा स्मरण रखना होगा कि भगवान् के मातृत्व की दो प्रकार से कल्पना की गयी है— विद्या माया तथा अविद्या माया। उसकी इस विद्या माया के रूप में पूजा की जाती है। इसी से वह लक्ष्मी-रूप में साधक की रक्षा करती हैं, पालन करती हैं, उसकी साधना को ऊर्ध्वगति देती हैं और उसके योग तथा साधना की रक्षा कर परिपोषण करती है।
योग-पथ में और अग्रसर होने पर माँ की महासरस्वती के रूप में आराधना करनी होती है। परब्रह्म का प्रथम प्रकाश जब सर्वप्रथम अव्यक्त से व्यक्त रूप धारण करता है, उस समय का माँ का यह रूप है और वह ब्रह्म के सर्वाधिक सन्निकट हैं। इस प्रथम अभिव्यक्ति के रूप में वह ज्ञानदायिनी हैं। वह जीव का परमात्मा अथवा परब्रह्म से योग कराती हैं और उसे परा ज्ञान प्रदान करती हैं। इससे वह उन्नत आत्म-चैतन्य अनुभव करता है। साधक उस समय माँ की विद्या माया के रूप में आराधना करता है जिससे वह जिस पथ से सृष्टि-राज्य में अवतरित हुआ है, माँ उसको पुनः ऊर्ध्वारोहण करने में स्थूल जगत् से मूल अव्यक्त तत्त्व तक जाने वाले ऊर्ध्वमुखी पथ पर प्रयाण करने में उसकी सहायक हों।
अष्ट-ऐश्वर्यशालिनी लक्ष्मी
महालक्ष्मी के अविद्या माया-रूपी प्रापंचिक स्वरूप का हम प्रथम विचार करें। यह अविद्या माया ही परब्रह्म से प्रकट हुई इस सृष्टि का परिरक्षण करती हैं। इस पार्थिव
जगत् में सफल तथा सौभाग्यशाली जीवन-यापन के लिए जो विविध वस्तुएँ आवश्यक हैं, वे सब अविद्या माया के ही स्वरूप हैं। महालक्ष्मी अष्ट-ऐश्वर्यशालिनी हैं। हिन्दू-जन उन्हें अष्टलक्ष्मी नाम से अभिहित करते हैं। जगत् में जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक वस्तु है खाद्य। स्थूल देह धारण करने वाले सभी प्राणी खाद्य से ही पोषण प्राप्त कर जीते हैं। यह खाद्य प्रमुख रूप से कृषिजात अन्न है। अन्न को धान्य कहते हैं। इसी से माँ की 'धान्य लक्ष्मी' के रूप में पूजा होती है।
हम सब देखते हैं कि कृषक तथा अन्य सभी लोग वर्ष में शस्य-लवन के दिनों में एक विशेष तथा निश्चित दिवस को नूतन धान के गुच्छे की पूजा करते हैं। उस दिन आनन्दोत्सव मनाते हैं। खेत में उगे नूतन शस्य के प्रथम बार काटने के समय उसे लवन कर बड़े समारोह तथा गान, वाद्य सहित घर ले जाते हैं और यथाविहित भाव से देवोचित पूजा करते हैं। इस भाँति माँ जीवन धारण के एक अतीव महत्त्वशाली साधन, धान्य के रूप में आराधित होती हैं और अपने इस रूप में वह हमारे इस सम्पूर्ण मानव-जगत् में प्रकट हैं।
दूसरे, समाज में चाहे वह अन्तर्देशीय हो या अन्तर्राष्ट्रीय, मनुष्य के सभी व्यवहारों के लिए सम्पत्ति अथवा धन की नितान्त आवश्यकता होती है। सम्पत्ति के बिना सुख, सौभाग्य तथा सफलता लाभ सम्भव नहीं है। धन के बिना वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए धन को भी लक्ष्मी माता का एक स्वरूप माना जाता है। धन का अर्थ किसी भी प्रकार की सम्पत्ति, मुद्रा, पण्य वस्तु प्रभृति सम्पूर्ण प्रकार की मूल्यवान् वस्तुएँ ही लेना चाहिए। इस भाव से समाज में धन भी सम्मानित व पूजित है।
भारत में माता जी के भिन्न-भिन्न स्वरूपों की भिन्न-भिन्न वर्गों में पूजा होती है। हिन्दू-समाज वर्णाश्रम की सुन्दर व्यवस्था पर अवस्थित है। समाज के कार्य के लिए श्रम-विभाग कर दिया गया है और राष्ट्र-जीवन के भिन्न-भिन्न अंगों की सँभाल भिन्न-भिन्न जातियों को सौंपी गयी है। माँ की धान्य-लक्ष्मी, धन-लक्ष्मी, विद्या- लक्ष्मी, धैर्य-लक्ष्मी, जय-लक्ष्मी, वीर्य-लक्ष्मी, राज-लक्ष्मी और सौभाग्य-लक्ष्मी- अष्ट-विध रूप में पूजा की जाती है।
जीवन-रक्षक अन्न में माता जी की धान्य-लक्ष्मी के रूप में तथा सम्पत्ति में माता जी की धन-लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है। इस संसार में सुखी तथा सभ्य जीवन-यापन के लिए कला और विज्ञान बहुत आवश्यक हैं। इन्हें अपरा विद्या कहा जाता है। इस अपरा विद्या में माता जी का विद्या-लक्ष्मी-स्वरूप में पूजन किया जाता है। सम्पत्ति तथा ज्ञान के सदुपयोग के लिए आवश्यक साहस में माता जी की धैर्य-लक्ष्मी के रूप में और जीवनी शक्ति में माँ की वीर्य-लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है। राज-सत्ता में राज-लक्ष्मी की भावना कर उनका पूजन किया जाता है। विपरीत परिस्थितियों तथा सफल, वैभवशाली और सुखी जीवन में बाधा डालने वाले अन्तरायों पर विजय दिलाने वाली शक्ति में जय-लक्ष्मी के रूप में और सर्व क्षेत्रों में. समृद्धि में सौभाग्य-लक्ष्मी के रूप में माँ की पूजा की जाती है। पालक व पोषक शक्ति-रूपा माँ लक्ष्मी इस मानव-लोक में इन अष्टविध रूपों में प्रकाशित हैं। क्षत्रिय युद्ध में विजयदायी अस्त्रों के रूप में माँ की पूजा करते हैं। उनके लिए खङ्गादि विजय-शस्त्र महालक्ष्मी के ही रूप हैं।
समाज की वर्ण-व्यवस्था में तृतीय स्थान वैश्यों का है। ये लोग वाणिज्य व व्यवसाय करते हैं और महालक्ष्मी की धन-रूप में पूजा करते हैं। इस संसार में धन ही सर्वोपरि शक्ति है। अतः उन्होंने माँ की धन-रूप में पूजा करने के लिए एक विशेष दिन निश्चित कर रखा है। लक्ष्मी-पूजा और दीपावली के दिनों में, विशेषकर बम्बई जैसे वैभवशाली नगरों में रुपयों का स्तूप बना कर उसकी साक्षात् माँ लक्ष्मी के रूप में वैसे ही पूजा करते हैं जैसे भावुक हिन्दू देव-देवियों की करते हैं।
समाज की वर्ण-व्यवस्था का चतुर्थ अंग शूद्र हैं। वे शस्य उत्पादन करते हैं और शस्य की ही लक्ष्मी-रूप में पूजा करते हैं। ब्राह्मण ज्ञान के ट्रस्टी (अमानतदार) माने जाते हैं। इनका काम लोगों को ज्ञान प्रदान करना है। ये माँ की विद्या तथा पुस्तक-रूप में पूजा करते हैं। आयुध-पूजा के दिन सब प्रकार के यन्त्रों व प्राण-रक्षक शस्त्रों की भी पूजा का प्रचलन है। इस भाँति हिन्दू-समाज में मानव-समाज के रक्षक तथा पालक-रूप में भगवान् के मातृ-स्वरूप का दर्शन विविध रूपों में होता है।
लक्ष्मी के प्रति साधक का भाव
इस प्रकार एक श्रद्धालु हिन्दू, जो शक्ति इस भौतिक जगत् में सभी प्राणियों का पालन-पोषण करती है, उस मातृ-शक्ति को अपने भौतिक जीवन के लिए देवी का एक महत्त्वपूर्ण आविर्भाव मानता है। यह उसकी बुद्धियुक्त यथार्थवादिता का परिचायक है। इस भूलोक में सुख-सम्पत्ति से समृद्ध जागतिक जीवन के रक्षण तथा पोषण करने में जो-जो तत्त्व सहायक बनते हैं, उन सबको वह इस भौतिक जगत् में दिव्य शक्ति का प्रकट स्वरूप मानता है और ऐसा ही उनका मूल्यांकन करता है। इस भाँति हम इस संसार की समस्त सुन्दर वस्तुओं के प्रति उसके यथार्थवादी भाव को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि परब्रह्म अथवा चरम सत्ता की शाश्वत खोज भी प्रत्येक निष्ठावान् हिन्दू की आन्तर चेतना का एक अविभाज्य अंग है।
जो हिन्दू जगत् की सम्पत्ति तथा अन्य समस्त सुन्दर वस्तुओं को लक्ष्मी के प्रतीक-रूप में श्रद्धापूर्वक पूजता है, वही मन एवं प्राण से यह भी स्वीकार करता है कि जब भी उसके अन्तर में दिव्यानुभूति की अभीप्सा उदय होती है, तो व्यावहारिक जगत् के लिए नित्यप्रति अतीव आवश्यक लक्ष्मी के इस रूप की उपासना को दृढ़तापूर्वक तिलांजलि दे उससे विरत हो जाता है। इस भाँति वह इस जगत् के भौतिक पदार्थों से मुख मोड़ लेता है और सम्पत्ति का त्याग कर त्याग का पथ अवलम्बन करता है। वह स्वीकार करता है कि जब तक व्यक्ति तृष्णा तथा उसकी पूर्ति में रत है, तब तक जागतिक पदार्थों में वर्तमान पराशक्ति के स्वरूप को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा; परन्तु जिस क्षण उसकी वासना-पूर्ति की दौड़ समाप्त हो जाती है, जगत् के पदार्थों की विनश्वरता, क्षणिकता तथा अनित्यता उसे मालूम हो जाती है तथा जिस क्षण उसका मन अक्षर वस्तुओं में लगता है, उस क्षण वह माता के उस लक्ष्मी-स्वरूप को अन्तिम विदायी दे कर उनके अपर स्वरूप अर्थात् विद्या माया की आराधना आरम्भ कर देता है। उस समय वह माँ के समीप प्रार्थना करता है-"माँ, मुझे अपने धन, सौभाग्य, पारिवारिक सुख तथा सांसारिक श्रेष्ठ पदार्थों की मोहकारी माया-शक्ति के प्रभाव से मुक्ति दान कर।" इस भाँति वह अविद्या माया रूपी लक्ष्मी की पूजा से विचारपूर्वक विलग हो जाता है। साधक तथा सामान्य सांसारिक प्राणी में यही मुख्य अन्तर है। दोनों के एक ही देवी की पूजा के भिन्न रूप हैं और उनके अन्तर में भिन्न तत्त्व हैं।
सांसारिक मनुष्य भी माँ की उपासना करता है और संसार से विरक्त साधक भी लक्ष्मी की उपासना करता है। बाह्य दृष्टि से ये दोनों पूजाएँ एक ही समान प्रतीत होती हैं; परन्तु जब एक बार लक्ष्मी की विद्या तथा अविद्या माया का रहस्य समझ में आ गया, तब सतही तल से नीचे गम्भीरता में उतरने पर विदित होता है कि एक ही माता लक्ष्मी देवी की उपासना में आकाश-पाताल का अन्तर है। सांसारिक कामनाओं एवं तृष्णाओं से बद्ध एक सांसारिक मनुष्य एवं सांसारिक इच्छाओं तथा तृष्णाओं का सर्वथा त्याग करने वाले एक तत्त्व-जिज्ञासु के दृष्टिकोण में बहुत ही अन्तर है।
माँ की मूर्ति एक है, माँ भी एक हैं, सौभाग्यदायिनी तथा रक्षाकारिणी-रूपा लक्ष्मी का स्वरूप सदा ही मंगलमय रहता है। वह धवल परिधान से सुशोभित हैं। वह स्वर्ण आभूषण धारण किये हुए हैं। शक्ति तथा ऐश्वर्य का प्रतीक-रूप हस्ती उनके पार्श्व में बैठा हुआ है। वह पद्मासनस्थ हैं और उनके उभय हाथों में दो प्रफुल्लित पद्म हैं। इन पद्मों का रहस्य तब प्रकट होगा, जब हम विचार करेंगे कि ये किसके प्रतीक हैं। पूर्ण प्रस्फुटित पद्म सर्वांगीण विकास की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं। इसी प्रकार हाथी भी दो विषय प्रकट करते हैं-सौभाग्य की चरमावस्था, राजकीय वैभव व राज्य-ऐश्वर्य तथा परा ज्ञान। हाथी ज्ञान की पराकाष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥'
(दुर्गासप्तशती : ५-५८)
जो देवी लक्ष्मी स्वरूप से व्याप्त सर्व भूतों में माँ।
नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है नमो नम: ।।
पंचम रात्रि
ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः
सौभाग्य का पथ
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि ।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ।।'
(दुर्गासप्तशती : ११-११)
स्रष्टा, पालक, संहारक जीवों में शाश्वत शक्ति माँ।
गुणी गुणाश्रय नारायणि को नमस्कार है, तुम्हें नमः॥
हमारे जीवन का जीवन, हमारे अस्तित्व का एकमात्र आधार, हमारी सत्ता का सारतत्त्व, हमारी चेतना का अन्तर्तम स्थल, हमारे जीवन का ध्येय व अन्तिम गन्तव्य-स्थल, हमारी योग-साधना का सुफल, शुद्ध सत्-चित्-आनन्द-स्वरूपा भगवती माँ तुमको प्रणाम! माँ, तुम्हारे दुर्गा, लक्ष्मी तथा सरस्वती-रूप में तुम्हें बार-बार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारी कृपा हम सब पर हो!
इस भूतल पर जीवन धारण तथा वहन केवल लक्ष्मी-रूपा माँ की कृपा से ही सम्भव है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद न होने से यह संसार केवल दुःख की यात्रा ही होता, यह अश्श्रु-सरिता में परिणत होता। संसार के समस्त पदार्थ ही नाशवान् हैं और माँ दुर्गा सर्वव्यापक रूप में उनमें अवस्थान करती हैं। प्राणी जब संसार में जन्म ले कर प्रथम दिवस के प्रकाश का दर्शन करता है, तब से ले कर मृत्यु के समय चिर-निद्रा में लेटने तक काल उसका पीछा करता रहता है। उसे पग-पग पर मृत्यु के दर्शन होते हैं। वस्तुतः इस लोक का जीवन दुःख और मृत्यु का ही जीवन है। अपने शुभ्र, तेजोमयी तथा आनन्ददायिनी लक्ष्मी रूप में माँ कष्ट व विनाश से परिव्याप्त हमारे इस जागतिक जीवन में प्रकाश, सौमनस्य, आनन्द, सौभाग्य और सुख को विविध मधुर रूपों के द्वारा सन्तुलन ला कर उसे सहनीय बना देती हैं। मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में माँ अपने मंगलमय स्वरूप में विराजती हैं। माता जी कल्याणी हैं, मंगलमयी हैं, सौभाग्यदायिनी हैं। राष्ट्र के बृहत्तर परिवेश के मध्य में तथा व्यक्ति के क्षुद्र पारिवारिक क्षेत्र में लक्ष्मी जी अपने उज्ज्वल व आनन्दमय रूप में आविर्भूत होती हैं जिससे उनके प्रकाश, उनकी मनोहरता तथा उनकी कृपा से सबका जीवन टिका रहता है। इस प्रकार माँ दुर्गा तथा माँ लक्ष्मी इस सांसारिक जीवन में सन्तुलन की रक्षा कर जीव के इस अनित्य तथा क्षणस्थायी जीवन के कठोर सत्य को विस्मृत करा देती हैं जिससे उसे जीवन के कुछ सुष्ट पदार्थों के उपभोग से जीवन में किंचित् सुख तथा आनन्द प्राप्त करना सम्भव हो पाता है।
राष्ट्र के गौरव-चिह्न
इन उभय क्षेत्रों में माँ लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप के विषय की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास अतीव उपयोगी तथा रोचक कार्य है। इसको जान कर ही हम इन क्षेत्रों में वर्तमान महालक्ष्मी की उपस्थिति बनाये रखने के कार्य में बुद्धिपूर्वक अग्रसर होंगे जिससे हम अपने लौकिक जीवन को सुख और समृद्धि से पूर्ण कर सकते हैं। मनुष्य के सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन के बृहत् क्षेत्र में माता जी ऐसी शक्ति के रूपों में प्रकट होती हैं जो दुर्गा माता की भीषण तथा संहारकारिणी शक्ति का प्रतिकार करती तथा उसके व्यापक प्रभाव में सन्तुलन लाती हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि जगत् में जीवन के रक्षार्थ दुर्गा माता अपने अत्यावश्यक विनाशकारी तथा प्रलयकारी स्वरूप में किस प्रकार प्रकट होती हैं। माता जी की यह कल्याणकारी विध्वस की योजना न होती, तो इहलौकिक जीवन नितान्त अव्यवस्था तथा विनाश में, अनिष्ट और संकट में ही समाप्त हो जाता। इस भाँति दुर्गा माता युद्ध, महामारी, दुष्काल तथा बाढ़, अग्नि, भूकम्प जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के विकराल रूप से संहार करती हैं। दुर्गा माता संहार करती हैं जीवन की रक्षा के लिए, जीवन का सातत्य बनाये रखने के लिए। अपने जीवन में लक्ष्मी जी अपने दुर्गा माता के स्वरूप में किये हुए कार्यों के प्रतिकार करने तथा सन्तुलन स्थापित करने के लिए युद्ध के बदले शान्ति-रूप में प्रकट होती हैं। जब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तब जगत् में सर्वत्र शान्ति होती है, जाति-जाति तथा राष्ट्र-राष्ट्र में शान्ति का प्रसार होता है, गृह-युद्ध से छुटकारा मिलता है। लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने पर समृद्धि होती है, उर्वरता का प्राचुर्य होता है तथा जगत् शस्य से पूर्ण होता है। रोग, कष्ट और अशान्ति दूर होते हैं। समाज के ऊपर अनुग्रह कर माँ शिशुओं तथा स्त्रियों को स्वास्थ्य प्रदान करती तथा उनका मंगल और कल्याण करती हैं। राष्ट्र के स्वास्थ्य-स्तर को उन्नत करती हैं। चिकित्सीय व्यवसाय, चिकित्सालय, अग्निशामक दल, आरक्षी दल आदि संरक्षक स्वरूप लक्ष्मी माता द्वारा भगवान् विष्णु की पालक-शक्ति प्रकट होती हैं और प्राकृतिक प्रकोप का प्रतिकार करती और मनुष्य के जीवन तथा उसकी सम्पत्ति की रक्षा करती हैं। अतः राजनयिकों, शासनकर्ताओं तथा सामाजिक नेताओं के लिए ये संरक्षक रूप सामाजिक संरचना में लक्ष्मी की विद्यमानता के सूचक हैं।
जहाँ इन वस्तुओं की उपेक्षा की जाती है, वहाँ हम देखते हैं कि लोगों का सुख नष्ट हो जाता है, उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा ऐसे समाज और राष्ट्र का परित्याग कर समृद्धि चली जाती है। इसी से प्राचीन स्मृतिकारों ने यह विधान कर दिया था कि प्रत्येक निष्ठावान् प्रशासक को माता जी के इन स्वरूपों का ध्यान रखना चाहिए तथा माता लक्ष्मी का जिन वस्तुओं द्वारा आविर्भाव होता है, उन वस्तुओं की समाज में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसके लिए उसे श्रमपूर्वक यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। देवालय, विद्यालय, क्रीड़ास्थल, उद्यान, पुष्पवाटिका, सरोवर इत्यादि मानव-समाज के समस्त पदार्थ विष्णु-शक्ति लक्ष्मी जी के प्रकट स्वरूप हैं। इन सब प्रतीकों द्वारा ही माता लक्ष्मी व्यक्त होती हैं। इसी से हम देखते हैं कि इस धर्मभूमि भारत में मन्दिर के बिना कोई भी स्थान नहीं है। भले ही वह सामान्य नन्हाँ-सा ग्राम हो, उसमें कुछ इने-गिने छप्पर के घर हों; पर वहाँ पर ग्राम-देवता अवश्य होंगे, भले ही उनके लिए सामान्य पक्का मन्दिर न हो और वह किसी वृक्ष की छाया में ही विराजते हों, पर ग्रामवासी उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। जिस ग्राम में ऐसा मन्दिर नहीं होता, वहाँ कोई भी धर्मानुरागी पुरुष पाँव नहीं रखेगा। वह कहेगा कि वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं है। वह उससे दूर रहता है। जिस स्थान में मनुष्यों तथा पशुओं के पीने के जल की सुव्यवस्था नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करतीं। पुण्यात्मा जन उस स्थान से दूर चले जायेंगे। इसी से सभी धार्मिक महानुभाव, सम्पत्तिवान् उदार गृहस्थ जन देश भर में स्थान-स्थान पर लक्ष्मी के इस प्रकार के व्यक्त स्वरूप की स्थापना करने में अपनी ईश्वर-प्रदत्त सम्पत्ति का सदुपयोग करते हैं। वृक्षारोपण करना, कूप तथा तड़ाग खुदवाना, उद्यान तथा क्रीड़ास्थल दान करना, जहाँ मन्दिर न हों वहाँ मन्दिर निर्माण करवाना और जीर्ण-शीर्ण मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाना, यात्रियों की विश्रान्ति के लिए धर्मशाला बनवाना, श्रान्त यात्रियों, पुण्यात्मा सन्तों, भगवद्-भक्तों, साधुओं, अभ्यागतों तथा साधकों के लिए अन्नक्षेत्र खोलना-ये सब धर्म-कार्य माने जाते थे और अब भी माने जाते हैं। यह महान् पुण्य-कार्य है जिससे दाता को इस भूलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। शिक्षा अथवा ज्ञान-दान भी अष्टलक्ष्मी में से एक विद्या-लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस भाँति हमारे स्मृतिकारों ने महालक्ष्मी का विविध रूपों में इन स्थानों में आविर्भाव माना है। अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह समाज तथा देश में इनकी वृद्धि का प्रयास करे, जिससे देश में समृद्धि की अवस्था सदा बनी रहे।
राष्ट्रीय नेताओं का सर्वोपरि कर्तव्य
किसी भी देश अथवा राष्ट्र के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रशासक के लिए इतना ही मान लेना पर्याप्त न होगा कि लक्ष्मी के इन स्वरूपों की केवल रक्षा तथा वृद्धि ही उनका प्राथमिक कार्य व कर्तव्य है। उन्हें इसे भी सदा स्मरण रखना होगा कि इनकी रक्षा और वृद्धि में ही सब लोगों के कल्याण तथा सुख का बीज समाहित है। इस भाँति व्यक्ति को जब इस जगत् की वास्तविकता का भान है तथा जब तक वह बाह्य वस्तुओं की सत्यता अनुभव करता है, तब तक वह इन वस्तुओं की अवगणना न करे, यह देखना उसका कर्तव्य है। हिन्दू-धर्म का खोटा स्वीयकरण, व्यक्ति के कर्तव्य के विषय में त्रुटिपूर्ण विचार, उपनिषदों के वेदान्तिक ज्ञान की अपच-इन विविध कारणों से हिन्दू-जाति के शताब्दियों पुराने यथार्थ स्वरूप की हम दुर्भाग्यपूर्ण उपेक्षा करने लगे। इसके परिणाम-स्वरूप वैराग्य के, भगवत्साक्षात्कार के तथा संसार की अनित्यता के अपरिपक्व विचारों को ले कर समस्त भारतवासी महालक्ष्मी के इन स्वरूपों के परिरक्षण के प्रति उदासीन बन गये। वे यह मानते थे कि ये सब केवल माया के क्षेत्र की वस्तुएँ हैं और इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है एवं तथाकथित पारलौकिक उन्नति के लिए उनसे मुख मोड़ लेने में ही दार्शनिक ज्ञानमय जीवन की पराकाष्ठा है। बाह्य जगत् में लक्ष्मी जी के इन स्वरूपों के प्रति इस प्रकार की उदासीन वृत्ति रखने के लिए हिन्दू-जाति को भारी मूल्य चुकाना पड़ा। माता जी के अनमोल स्वरूप-रूपी देश की स्वतन्त्रता, समृद्धि तथा राष्ट्रीय गौरव हम खो बैठे। जबसे हिन्दू-जाति के अधिकांश लोगों ने तत्त्वज्ञान के भूल-भरे विचारों के कारण महालक्ष्मी जी को त्याग दिया तथा बाह्य जीवन में दृढ़ यथार्थवाद तथा व्यावहारिक आदर्शवाद के रूप में उनकी उपासना को तिलांजलि दे दी, तभी से माता जी ने हिन्दू राष्ट्र को त्याग दिया। इसी से शिक्षा की उपेक्षा की गयी तथा इस संसार के अन्य सभी सामाजिक कार्यों की भी यह मान कर अवगणना की गयी कि वे अज्ञानजन्य हैं, अतः उनका सम्पादन अनुपयुक्त है। सृष्टि-रचना के स्थूल स्तर पर शारीरिक चेतना से पूर्णतया आबद्ध मनुष्य ने भौतिक जगत् की वास्तविकताओं से अपने नेत्र बन्द कर लिए तथा ये सभी पदार्थ क्षणिक तथा नाशवान् हैं, ऐसी घोषणा कर उन्हें त्याग देने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हम पर लक्ष्मी जी की विरोधी शक्ति तामस प्रकृति का आधिपत्य हो गया, जिससे हमें दो शतकों तक दासता झेलनी पड़ी। जो बाह्य जगत् में लक्ष्मी जी के सही अर्थों में उत्तम उपासक थे, उनका दास बनना पड़ा। अँगरेज लोग लक्ष्मी जी की अर्चना सुचारु रूप से करते थे, अतः भारतवर्ष में जो-कुछ श्रेष्ठ था, जो वैभवप्रदायक तत्त्व थे, वे सब पाश्चात्य जगत् को चले गये; क्योंकि वे लोग भौतिकवादी होते हुए भी लक्ष्मी जी के उपासक थे। जब आधुनिक भारत के सन्तों तथा महान् विचारकों ने समझा कि तामस के अधीन बन कर हमने लक्ष्मी जी की अवगणना की है और यह अवगणना ही भारत की समस्या के मूल में है, तब उन लोगों ने तत्काल ही हिन्दू-राष्ट्र को गतिशील सामाजिक तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया। भारत के इन महान् उद्धारकों ने हिन्दू-राष्ट्र को अपनी तमोनिद्रा से जागने, निःस्वार्थ सेवा में निमग्न होने तथा जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण तथा अभिवृत्ति अपनाने के लिए शंख-घोष किया। इस भाँति नव-निर्माण आया तथा तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी अपरिपक्व तथा सदोष विचार मनुष्य के मस्तिष्क से निकाल बाहर किये गये। उन्हें यह भी समझाया गया कि जब तक उनके लिए अपने शरीर की सत्यता बनी हुई है तथा जब तक वे चेतना के ऊर्ध्वारोहण की, आत्म-विकास की ऐसी स्थिति तक नहीं पहुँच जाते जहाँ अपने हृदय के अन्तर्तम प्रकोष्ठ में वास्तविक रूप में यह अनुभव नहीं कर पाते कि यह संसार मात्र क्षणिक स्वप्न है और अव्यक्त ही एकमात्र चरम सत्य है, तब तक उन्हें माता जी का कर्मनिष्ठ उपासक बना रहना चाहिए। अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बहुत बार हम यह मानने की भूल कर बैठते हैं कि हम बहुत ही ऊँची आध्यात्मिक भूमिका में पहुँच गये हैं। इसके परिणाम-स्वरूप जिन वस्तुओं की हमें अवगणना नहीं करनी चाहिए, उनकी अवगणना कर बैठते हैं। कालान्तर में जिन वस्तुओं का त्याग करना है, वे ही प्रारम्भ में तो उच्च से उच्चतर आरोहण के लिए क्रमिक सोपान के समान होती हैं। तमस् से उद्भूत उपेक्षा-वृत्ति जिसे हम भूल से तत्त्वज्ञान तथा त्याग मान बैठे थे, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किये जाने पर हम उसे दूर कर अब रजोगुण के युग में प्रवेश कर चुके हैं। समग्र देश तथा समाज के कल्याण की उत्साहपूर्ण प्रवृत्तियों में लग जाने के लिए भारत देश तथा हिन्दू-समाज को झकझोर कर जागृत कर दिया गया है। इसमें रजोगुण की चंचलता की प्रधानता हम अनुभव कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ चिह्न हैं और यदि ये प्रवृत्तियाँ चालू रहें तथा लक्ष्मी जी अपने अविद्या-माया-स्वरूप में हमारी विशाल दृष्टि तथा ज्ञान को आच्छादित न कर लें, तो हिन्दू-जाति आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा पर अवश्य पहुँच जायेगी।
कठोर चेतावनी
इस भाँति एक व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में 'वह शरीर नहीं है, वरन् शरीर और मन से परे शुद्ध आत्मा है' यह सत्य आत्म-साक्षात्कार की अन्तिम अवस्था में भले ही सच हो, पर यदि कोई साधक मूर्खतावश अपनी आध्यात्मिक साधना का आरम्भ इस मान्यता से करता है, तो उसे शीघ्र ही पश्चात्ताप करना होगा; क्योंकि इस भौतिक जगत् के नियम बहुत ही कठोर हैं और यदि उनका उल्लंघन किया जाये, तो उसका मूल्य तुरन्त ही चुकाना होता है। यदि कोई वेदान्तिक भावों में ऊँची उड़ान भरता है और वह आत्म-चैतन्य की परमोच्च अवस्था को प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसके समस्त कर्तव्य शेष हो चुके हैं, ऐसा मान कर अपने शरीर की उपेक्षा करता है और उसे उचित पोषण तथा विश्राम दे कर स्वास्थ्य ठीक नहीं रखता, तो योग साधना के लिए प्राप्त इस सर्वोत्कृष्ट साधन 'मानव-शरीर' को अपूरणीय क्षति पहुँचती है। अति-आकांक्षित चित्तशुद्धि तथा चरित्र की निर्मलता जो निःस्वार्थ सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, उस सेवा का एकमात्र साधन यह मानव शरीर रोगग्रस्त होने से उसकी साधना की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी दशा में एकमात्र भगवत्कृपा ही उसे बचा सकती है। उसे स्वयं भी अपनी भूलों को सुधारने का प्रयत्न करना होगा।
जिस भाँति व्यक्तिगत जीवन में, जिस देह से साधना कर उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुँचना होता है, उस देह की प्रारम्भ से ही अवगणना करने से अवांछनीय परिणाम होते हैं, उसी भाँति तामस प्रवृत्तियों में पतित होने पर राष्ट्रीय जीवन में भी होता है। भारतीय समाज को इस बात का विचार प्रारम्भ में ही आना आवश्यक था और इससे बचना चाहिए था; परन्तु उसने बहुत ही कड़वे अनुभव के पश्चात् शिक्षा ग्रहण की। अब हमारे नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञ पुरुषों तथा अपने पूज्य गुरुदेव जैसे आध्यात्मिक उपदेशकों ने धर्म तथा निःस्वार्थ सेवा पर आधारित सक्रिय प्रवृत्तियों का अभिनन्दनीय कार्य प्रारम्भ किया है, जिससे समाज तथा राष्ट्र में नव-निर्माण की लहर दौड़ जायेगी। इसके परिणाम स्वरूप माता सरस्वती के साम्राज्य तक पहुँचने के लिए आवश्यक शान्ति, समृद्धि, राष्ट्रीय आरोग्य तथा उन्नति, राष्ट्रीय साक्षरता तथा सभी को उच्च शिक्षा प्राप्ति की स्थिति आयेगी, जिससे राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक नव-निर्माण शक्य हो सकेगा। इसका कारण यह है कि समाज तथा राष्ट्र में लक्ष्मी माँ के व्यापक आविर्भाव के बिना उच्च आध्यात्मिक ज्ञान-स्वरूपा सरस्वती के आविर्भाव की आशा नहीं की जा सकती; क्योंकि यह कहा जाता है कि क्षुधित उदर और नग्न शरीर वाले व्यक्ति को धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अतएव, राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन की समस्याओं के प्रति हमारी दृष्टि वास्तविक होनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र के लोगों को लक्ष्मी के ऐसे स्वरूप प्रदान करने होंगे, जिनसे वे स्वस्थ तथा सुखी जीवन-यापन कर सकें। सर्वतोमुखी समृद्धि, साक्षरता तथा स्वास्थ्य के सुष्ट वातावरण में ही उच्चतर आध्यात्मिक जीवन जीने की आकांक्षा अंकुरित होगी। ये आकांक्षाएँ हममें विद्यमान हैं, पर वे सुप्त भाव में हैं। राष्ट्र तथा समाज में लक्ष्मी के अभाव के कारण उन्हें लोगों के हृदय में प्रकाश में आने का सुयोग नहीं मिलता, क्योंकि दारिद्रय से उच्च आकांक्षाएँ कुण्ठित हो जाती हैं। जब क्षुधा उदर को पीड़ित कर रही हो, तो उच्च आदर्शों का विचार उदय नहीं होता।
विष्णु-शक्ति लक्ष्मी के इन प्रकट स्वरूपों के अपने विशिष्ट गुण हैं और प्रत्येक जाति व राष्ट्र के जीवन में उनका बड़ा महत्त्व है। अतः लक्ष्मी की उपासना में प्रतिष्ठित हो कर अन्त में विवेक तथा वैराग्य से एवं लक्ष्मी की सहायता से सरस्वती की आराधना करनी होती है। भारतीय संस्कृति की यही सनातन धारा है।
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः ।।
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम् ।।
(दुर्गासप्तशती :४-५)
पुण्यवान् के गृहों में रहती बन कर स्वयं जो लक्ष्मी माँ।
पापी के गृह दरिद्रता बन, बुद्धि बन सत्-जन हृद माँ।
सज्जन में श्रद्धा-स्वरूप जो, कुलोत्पन्न में लज्जा माँ।
देवी! करो विश्व का पालन, हम सब करते नमो नमः ।।
षष्ठ रात्रि
ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपल्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्
गृह तथा हृदय में सौभाग्यदायिनी देवी
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।
सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ।।
(दुर्गासप्तशती : ११-१२)
दीन आर्त जो शरण में आये उसकी रक्षा में रत माँ।
नारायणि! सबकी दुःखहर्ता, नमस्कार है तुम्हें नमः ।।
सृष्टि की रक्षाकारिणी देवी जननी तुम्हें कोटि-कोटि नमस्कार! विभिन्न नाम-रूपों के मध्य में जिस शक्ति का विकास है, माँ! तू ही उसका आधार है। तुम्हीं हमारे मन में साधन-शक्ति-रूप में आशा उदय करती हो, हमारे योग का परिरक्षण करती हो तथा हमारी चेतना में शुद्ध ज्ञान-रूप में प्रकाशित हो कर हमारी सम्पूर्ण सत्ता को उद्भासित करती हो। तुम्हें बार-बार प्रणाम।
श्री लक्ष्मी अथवा विष्णु-शक्ति अथवा नारायणी-रूप में माँ की आराधना का तृतीय पवित्र दिवस है। आज नवरात्र-पूजा के छठे दिवस को व्यक्ति के अन्तरंग गृह-क्षेत्र में तथा पारिवारिक जीवन में लक्ष्मी माता किस प्रकार प्रकट होती हैं, इस पर विचार करने का हमें दुर्लभ आशीर्वाद तथा सद्भाग्य प्राप्त हुआ है।
जिज्ञासु, साधक तथा मुमुक्षु के आन्तर जीवन में माँ दैवी सम्पद् के रूप में प्रकट होती हैं। इन दोनों स्वरूपों में माता जी हम सबके लिए विशेष रूप से तथा व्यावहारिक रूप से महत्त्व की हैं, क्योंकि माता जी के दोनों स्वरूपों का ज्ञान होने से ही माता जी किसमें विद्यमान हैं और किसमें विद्यमान नहीं हैं, यह हम जान सकते हैं, जिससे जिन वस्तुओं में माता जी विद्यमान हैं उनके परिरक्षण का प्रयास करेंगे और जिन पदार्थों में वे विद्यमान नहीं हैं, उनमें भी वे व्यक्त हों, इसके लिए हम अपना प्रयत्न चालू रखेंगे।
महिमामयी भारतीय नारी
इस गौरवशाली देश भारतवर्ष में गार्हस्थ्य जीवन में लक्ष्मी देवी की कल्पना सचमुच ही अद्भुत तथा अनुपम है। गृह ही लक्ष्मी जी का आवास-स्थान माना जाता है जहाँ माता जी पूजनीया गृहिणी के स्वरूप में व्यक्त होती हैं। गृह-जीवन तथा कुटुम्ब के सौख्य, सौभाग्य, मांगल्य तथा विकास की अधिष्ठात्री देवी को 'गृहलक्ष्मी' कहते हैं, यह हम सब जानते हैं। गृहलक्ष्मी साक्षात् लक्ष्मी देवी का साकार रूप है। हमारी भारतीय संस्कृति का यह अद्वितीय रूप पाश्चात्य देशों में दृष्टिगत नहीं होता। पाश्चात्य देशों में नारी अधिकांशतः पत्नी-रूप में, जीवनसंगिनी के रूप में पुरुष के समान भागीदार मानी जाती है। इतना ही नहीं, वह सभी कार्यक्षेत्रों में पुरुष के साथ विशेषाधिकार की स्पर्धा करने के साथ ही न केवल अपने समानाधिकार की अपितु उससे भी आगे अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का भी आग्रह करती है। इसके विपरीत हिन्दू-हृदय में नारी माता है। सच्चे हिन्दू की चेतना में नारी का यह मातृरूप सदा निवास करता है। इस पुण्य-भूमि में जन्म-ग्रहण का यही सौभाग्य है; क्योंकि इस भावना द्वारा हम ईश्वर के मातृरूप का साक्षात्कार करने की उन्नत कक्षा तक आरोहण कर सकते हैं। यह मातृभाव अथवा सम्पूर्ण नारी-जाति में माता का दर्शन अपने मन और हृदय को पवित्र करने का साधन है। इसके द्वारा हम इतनी उन्नतावस्था को प्राप्त हो सकते हैं जहाँ दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठना सुलभ हो जाता है।
इस भाँति हिन्दू के लिए गृह लक्ष्मी का आलय है। इसी से हिन्दू-समाज में प्रत्येक गृह ही मांगल्य व श्री का मन्दिर है, गृहलक्ष्मी-रूपा लक्ष्मी का आवास-स्थल है। लक्ष्मी जी की शक्ति, महिमा तथा ओजस गृहलक्ष्मी में सतीत्व अथवा पातिव्रत्य- धर्म के रूप में प्रकाशित होते हैं। इससे ही उनका ऐश्वर्य, यश तथा आन्तरिक प्रकाश गठित होता है। गृहलक्ष्मी की यह शक्ति विश्व-भर में अद्वितीय है। एक 'पातिव्रत्य' शब्द में ही स्त्री-धर्म की सम्पूर्ण भावना, सम्पूर्ण कल्पना समाहित है। साधक तथा जिज्ञासु के आध्यात्मिक जीवन में, योग के क्षेत्र में जो स्थान गुरु का है गृहलक्ष्मी के गृह-क्षेत्र में वही स्थान उसके पतिदेव का है।
त्वं हि विष्णुर्विरंचिस्त्वं त्वंच देवो महेश्वरः ।
त्वमेव शक्तिरूपोऽसि निर्गुणस्त्वं सनातनः ।।'
तुम्हीं विष्णु हो, तुम विरंचि हो, तुम्हीं महेश्वर हे गुरुदेव ।
शक्तिरूप हो, तुम निर्गुण हो और सनातन हो गुरुदेव ।।
इस श्लोक के कथनानुसार साधक जिस प्रकार गुरु को साक्षात् भगवान् समझता है, पत्नी भी अपने पतिदेव को वैसा ही समझती है। स्त्री के लिए पातिव्रत्य ही इस जीवन में अर्जनीय श्रेष्ठतम सम्पत्ति है। इससे वह केवल एक असाधारण नारी बनती है, इतनी ही बात नहीं है, वह इस संसार में साक्षात् देवी के समान स्थान पाती है; क्योंकि सतीत्व माँ लक्ष्मी की ही एक शक्ति-विशेष है। इसके साथ ही इस आन्तरिक गुण सतीत्व के बाह्य अभिव्यक्तिकरण का रूप शील है। हिन्दू-नारी के लिए शील उसका अलंकार-स्वरूप है। वह दूसरे पुरुषों को देखने और अपने को दूसरे पुरुषों को दिखाने की चिन्ता नहीं करती। यह एक उन्माद है, रोग है जो वर्तमान युग में खूब विकसित हो रहा है। आज व्यक्ति यह चाहता है कि दूसरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। इस उद्देश्य से रंगीन वेशभूषा और अन्य प्रत्येक प्रसाधन, जो घोर अन्धकार में निमग्न व्यक्तियों के उपजाऊ मस्तिष्क ने आविष्कृत कर रखे हैं, का उपयोग किया जाता है जिससे कि दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यह शील जैसे उदात्त एवं श्रेष्ठ गुण के अपरोक्ष रूप से विपरीत या प्रतिकूल है। शील की अवहेलना करने तथा दूसरों को आकर्षित करने के उन्माद को प्रश्रय देने से लक्ष्मी देवी का अपमान है। इसी का नाम अलक्ष्मी है। यह बात सदा स्मरण रखनी है कि हिन्दू-आदर्शों में शील की रक्षा एक महद् गुण है। इसी गुण के माध्यम से भारतीय नारी के मध्य में माँ लक्ष्मी स्वयं ही आविर्भूत होती हैं।
लक्ष्मी गृह में गृहलक्ष्मी के व्यक्तित्व में वाणी व व्यवहार में सुशीलता, मधुरता तथा चारुता के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। नारी को कभी भी परुष नहीं होना चाहिए। हिन्दू-गृह की लक्ष्मी के श्रीमुख से कभी भी रूढ़ शब्द, कठोर वाणी और कर्कश वचन नहीं निकलने चाहिए। अपना आदर्श ही यही है; क्योंकि हिन्दू-भावना में चारुता और मधुरता गृहलक्ष्मी का अंग माना जाता है। लक्ष्मी को समादृत करने और उनके पूजन का एक रूप है कठोर वाणी का सर्वथा त्याग। यह बात सभी गृह-देवियों को स्मरण रखनी चाहिए; क्योंकि यही घर के सच्चे सुख, शान्ति और कल्याण के आविर्भाव में सहायक होता है।
मांगल्य-सूत्र, जो कि गृहलक्ष्मी का एक विशिष्ट चिह्न है, को धारण करने के अतिरिक्त दो अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ भी हैं जिनसे सभी को अलंकृत किया जाता है; किन्तु लोगों को इस प्रथा का सम्यक् ज्ञान नहीं है। हिन्दू-गृह में लक्ष्मी दो अन्य रूपों में भी विद्यमान रहती हैं अर्थात् वह आदर्श हिन्दू-नारी के अलंकार के दो रूपों में-पुष्प के रूप में और तिलक के रूप में विद्यमान रहती हैं। हिन्दू-नारी को तिलक के बिना कभी नहीं रहना चाहिए। मस्तक पर बड़े आकार का तिलक धारण करने का एक विशेष तात्पर्य और एक गम्भीर तथा आवश्यक कारण है जिससे लोग अवगत नहीं हैं। इस बात को निर्धान्त रूप से स्वीकार करना चाहिए कि तिलक को धारण करने की उभय रूप से अत्यधिक सच्ची आवश्यकता तथा महत्त्व है-सूक्ष्म रूप में उस स्त्री के लिए जो तिलक धारण करती है और स्थूल दृष्टि से उन लोगों के लिए जिन्हें व्यवहार-काल में उसके सम्पर्क में आना पड़ता है। इसी भाँति पुष्प धारण का भी अपना महत्त्व है। पुष्प लक्ष्मी के प्रकट रूप ही हैं, अतः उन्हें भी धारण करना चाहिए; किन्तु हमें कभी भी यह विस्मरण नहीं करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी विद्या माया और अविद्या माया-इन दोनों रूपों में ही कार्य करती हैं। अतः उनके इस अविद्या-स्वरूप की उपासना बड़ी ही सावधानी hat H करनी चाहिए और नित्यप्रति उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें अपने इस स्वरूप की क्रीड़ा से सुरक्षित रखें और अपने विद्या-रूप से हमारा कल्याण करें।
देवी लक्ष्मी गृहलक्ष्मी के रूप में अभिव्यक्त होने के अतिरिक्त पतिदेव के प्रति सतत पूज्य भाव रखने और पति के माध्यम से ईश्वर की निरन्तर स्वैच्छिक आत्मत्यागमयी सेवा द्वारा भी अभिव्यक्त होती है।
श्री लक्ष्मी जी स्वयं इस उत्कृष्ट पति-सेवा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वैष्णवों की विचारधारा में परमा माता वैकुण्ठाधिपति विष्णु की चिर-सेविका मानी गयी हैं। वह स्वयं सर्वदा भगवान् विष्णु की पद-सेवा में रत रहती हैं। श्री लक्ष्मी देवी सम्बन्धी यह धारणा अतीव महत्त्वपूर्ण है और प्रत्येक आदर्श हिन्दू-नारी को उचित है कि वह लक्ष्मी देवी के इस आदर्श को स्मरण रखे और उसे अपने निजी जीवन में चरितार्थ करे।
गृह में लक्ष्मी जी का आविर्भाव
यदि हम गृहलक्ष्मी के व्यक्तित्व से आगे बढ़ कर गृह के चारों ओर ध्यान दें तो पायेंगे कि स्वच्छता लक्ष्मी के आवास का एक महत्त्वपूर्ण रूप है। घर के पास धूलि और गन्दगी अलक्ष्मी का आवास है। दक्षिण भारत में इसे दारिद्र्य कहा जाता है।
इसके अनन्तर दीपक की बारी आती है। गोधूलि और सूर्यास्त का समय निकट आते ही हम देखते हैं कि प्रत्येक हिन्दू-घर में दीप प्रज्वलित कर उसे प्रणाम करते हैं। इस भाँति अन्धकार के आरम्भ होने से पूर्व ही धवल प्रकाश का आगमन होता है। इस प्रथा का प्रत्येक हिन्दू-घर में अनुसरण किया जाता है, क्योंकि लोगों की यह मान्यता है कि प्रकाश अथवा ज्योति गृहक्षेत्र में प्रकट होने वाली लक्ष्मी का एक स्वरूप है।
तदुपरान्त देव-देवी की पूजा को लें। देव-देवी की पूजा अत्यावश्यक है। जहाँ देवों की पूजा नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वह अविद्या-रूप में भले ही आ जाये; किन्तु जहाँ देव-पूजन नहीं होता, आपाततः ऐश्वर्य-लाभ होने पर भी, अन्त में उस घर से वैभव जाता रहेगा और दारिद्रय, दुःख और सन्ताप निश्चय ही अपना आधिपत्य जमायेंगे। यह एक आवश्यक बात है जिसे इस पुण्य-भूमि के जिन लोगों पर पाश्चात्य विचारधारा और पश्चिमी रहन-सहन का प्रभाव दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है, वे यदि वास्तव में अन्ततः अपना सुख और परिवार की समृद्धि चाहते हैं, तो स्मरण रखें और इससे सावधान रहें। देवों की पूजा करनी चाहिए। पुण्य-पर्व तथा परम्परागत त्योहारों को मनाना अपने गृह-जीवन का सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण भाग है। इस पवित्र देश में मनाये जाने वाले जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि उत्सवों की अवहेलना की गयी, तो उस घर में मंगल नहीं रहता, ऐसा हम कह सकते हैं।
दान : गृहस्थाश्रम में लक्ष्मी माँ का यह भी एक महत्त्वपूर्ण आविर्भाव है। गृहस्थ को तो अन्य तीनों आश्रम वालों के साथ उसके पास जो कुछ भी है, उसमें भागीदार बना कर उपभोग करने का अपूर्व सौभाग्य प्राप्त है। अध्ययन-रत निर्धन ब्रह्मचारी, परिव्राजक संन्यासी तथा सर्वस्व त्याग कर संन्यासाश्रम की पूर्व तैयारी रूप पवित्र जीवन-यापन करने वाले वानप्रस्थ-इन सबके निर्वाह का उत्तरदायित्व गृहस्थ पर है। इन तीनों आश्रमवासियों को दान देने का दुर्लभ सद्भाग्य द्वितीय आश्रमी गृहस्थ को ही प्राप्त है। इस अवसर का लाभ उठाने से गृहक्षेत्र में लक्ष्मी देवी का प्राकट्य होता है। दान-रूप में वह विष्णु भगवान् की पोषक शक्ति का कार्य करता है। इससे धर्म की रक्षा होती है और अन्य आश्रमों की परम्परा बनी रहती है।
आतिथ्य-सत्कार लक्ष्मी का एक महत्त्वपूर्ण स्वरूप है। जिस घर से अतिथि विमुख होता है, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करर्ती; परन्तु जहाँ याचक और अतिथि का स्वागत होता है, वहाँ लक्ष्मी पूर्ण ओजस से रहती हैं और घर को आशीर्वाद देती हैं। अतिथि-सत्कार, दानशीलता और उदारता-ये लक्ष्मी जी के महत्त्वपूर्ण स्वरूप हैं जिनका भावुक हिन्दू-गृहस्थ को श्रमपूर्वक धर्म-भाव से पालन करना चाहिए।
भारतीय गृह में और विशेषकर हिन्दू-गृह में अन्य दो वस्तुओं में भी माता लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। प्रथम वस्तु है तुलसी का पवित्र पौधा । तुलसी के पौधे के बिना कोई घर नहीं रहना चाहिए; क्योंकि इस भूतल पर तुलसी के पौधे के रूप में साक्षात् लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। परमात्मा की वह साक्षात् विभूति हैं। इस विषय में मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्रीय इस सम्बन्ध में बहुत सावधान रहते हैं। वे चाहे कहीं भी रहें, वे करोड़पति ही क्यों न हों, भले ही वे बड़े नगरों में भौतिकवाद के पर्यावरण में रहते हाँ, चार-पाँच मंजिलों वाले मकान में सैकड़ों किरायेदारों के साथ रहते हों, पर आप देखेंगे कि प्रत्येक महाराष्ट्रीय घर में मिट्टी का एक छोटा-सा पात्र होगा जिसमें तुलसी का पौधा उगा होगा। घर में प्रवेश करते ही तुलसी का दर्शन होगा। जिस गृह में इस विशिष्ट रूप में माता जी का पूजन होता है, उस घर को वह आशीर्वाद देती हैं। कोई भी महाराष्ट्रीय गृहलक्ष्मी तुलसी के पौधे को एक-दो पुष्प अर्पित किये बिना अथवा कर्पूर-आरती किये बिना अथवा एकाध प्रदक्षिणा किये बिना अथवा भावपूर्वक शिर झुका कर तुलसी देवी का वन्दन किये बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करती।
लक्ष्मी देवी का दूसरा स्वरूप जो दुर्भाग्य से सभी नगरों के हिन्दू-गृहों से तीव्र गति से विलुप्त होता जा रहा है, वह है गौमाता। एक-दो पीढ़ी पूर्व हिन्दू-घरों में प्रतिदिन गोमाता के पूजन की प्रथा प्रचलित थी। भावुक हिन्दू-गृहिणी गो-पूजा किये बिना भोजन नहीं करती थी। नगरों में अब गाय का दर्शन दुर्लभ हो गया है। समस्त दुग्ध दुग्धशालाओं से बोतलों में भर कर पहुँचाया जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप नगरों में से यह प्रथा प्रायः लुप्तप्राय हो चली है। एक हिन्दू-गृहलक्ष्मी के लिए नित्य गो-पूजन की प्रथा चालू रखना शक्य न हो, तो इसके प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे वर्ष में न्यूनातिन्यून एक या दो दिन अवश्यमेव गो-पूजन करने का निश्चय लेना चाहिए। वर्ष में एक विशेष दिन गो-पूजा के लिए पृथक् रखा गया है और उस दिन लोग जहाँ भी गाय मिलती है, वहीं उसकी पूजा की व्यवस्था करते हैं। पवित्र गोमाता, जो एक समय हिन्दू-मान्यतानुसार वैभव का एक महान् प्रतीक मानी जाती थी और जिस गोमाता में लक्ष्मी जी साक्षात् प्रकट रूप में विराजमान हैं, उस गोमाता की पूजा का अधिकाधिक अवसर प्रस्तुत करते रहना चाहिए। गृह में लक्ष्मी जी के आविर्भाव का इतना ही वर्णन पर्याप्त होगा।
साधक की आध्यात्मिक सम्पत्ति
अब हम इस विश्व में लक्ष्मी जी के सर्वश्रेष्ठ मोक्षदायी रूप का विचार करेंगे। माता जी अपने लक्ष्मी-स्वरूप में मुख्य रूप से रजोगुणी हैं; क्योंकि रजस् से ही क्रियाशीलता चालू रहती है। गतिशीलता की प्रक्रिया द्वारा ही जीवन का सातत्य बनाये रखा जा सकता है। इसी से माता जी रजोगुण का अंश भी रखती हैं; परन्तु माता जी की अन्तरतम गहराई में विशुद्ध सत्त्व का भण्डार भरा पड़ा है, क्योंकि विष्णु सत्त्वगुण-प्रधान हैं, सत्त्व के अंशी हैं और अन्ततः माता जी को अपने तृतीय स्वरूप, सरस्वती में विलीन होना है। हम जब लक्ष्मी तथा सरस्वती के प्रकट स्वरूप के मध्य की सीमा-रेखा पर पहुँचते हैं, तब माता लक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी-स्वरूप में प्रकट होती हैं।
जिस साधना द्वारा हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, वह माता जी का मोक्षलक्ष्मी-स्वरूप है। साधक के जीवन में माता जी इसी स्वरूप में प्रकट होती हैं। गीता जी के षोडश अध्याय में कतिपय मुख्य सद्गुणों का वर्णन है। इन सद्गुणों के रूप में माता जी व्यक्त होती हैं। अभीरुता, चित्तशुद्धि, ज्ञान और योग में निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपिशुनता, प्राणिमात्र पर दया, अलोलुपता, मृदुता, शील तथा अचंचलता-इन स्वरूपों में माता जी प्रकर होती हैं। यहाँ दो अतीव रोचत बातें ध्यान में रखनी हैं। अविद्या माया के रूप में जहाँ लक्ष्मी जी सम्पत्ति के रूप में प्रकट होती हैं, वहीं उसके आनुषंगिक सहवर्ती धन-लोभ, दम्भ, दर्प, धन-संग्रह की वृत्ति तथा धन के अभिमान-रूप में भी प्रकट होती है। भगवान् श्री कृष्ण आध्यात्मिक मार्ग की दैवी सम्पद् का बहुत अर्थपूर्ण वर्णन करते हैं। उसमें अविद्या माया के प्रकट स्वरूपों के साक्षात् विरोधी स्वरूपों का वर्णन है। इसी कारण गीता के षोडश अध्याय के द्वितीय श्लोक में अलोलुपता तथा अचंचलता का वर्णन पाया जाता है। साधक के हृदय में इन चौबीस प्रकार के दैवी सम्पद् के रूपों में लक्ष्मी माँ निवास करती हैं।
साधक के हृदय में शम तथा दम-ये दो सद्गुण प्रकट होते हैं। मन की चंचलता की विरोधी स्थिरता तथा सम्पत्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली स्वार्थ-वृत्ति की विरोधी निःस्वार्थ-वृत्ति का भी उद्भव होता है। साधक के हृदय में आज्ञाकारिता के महत्त्वपूर्ण स्वरूप में माता जी स्वयं प्रकट होती हैं, क्योंकि स्वयं माता जी महाविष्णु की आज्ञाकारिता की साकार रूप हैं। जिस भाँति माँ पातिव्रत्य तथा अपने स्वामी भगवान् विष्णु की सेवा में सम्पूर्ण समर्पण की सर्वश्रेष्ठ प्रतीक रूप मानी जाती हैं, उसी प्रकार माता जी साधक के हृदय में स्वयं स्फुरित गुरु-भक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। गुरु-भक्ति के साथ-ही-साथ अनन्य भाव से सर्वस्व समर्पण कर निःस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना भी साधक के हृदय में आविर्भूत होती है।
माता जी साधक के व्यक्तित्व में तीव्र निरीक्षण-शक्ति, सावधानी तथा जागरूकता के स्वरूप में प्रकट होती हैं। योग-मार्ग में विचरण के लिए इन सद्गुणों का होना अत्यन्त महत्त्व का है। साधक को प्रमादी नहीं होना चाहिए। जिनसे अमूल्य शिक्षाएँ प्राप्त होती हों, उन महत्त्वपूर्ण वस्तुओं को विस्मृत नहीं करना चाहिए। जीवन की इस महान् पाठशाला में केवल अनुभव द्वारा ही शिक्षा मिलने से तीव्र निरीक्षण-वृत्ति साधक के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। यदि साधक निरीक्षण द्वारा अनुभवों से ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से चूक जाता है, तो लक्ष्मी देवी के इस महत्वपूर्ण स्वरूप का उसे भान नहीं होता।
अनुशासन : साधक को आध्यात्मिक अनुशासनों का पालन करना चाहिए। यह शुभ लक्षण है। जिस भाँति माता जी अपने शक्ति-स्वरूप से हमें दृढ़ता तथा मनोबल का आवश्यक सद्गुण प्रदान करती हैं, उसी भाँति आत्म-संयम तथा दृढ़ मनोबल से संरक्षक-स्वरूप अनुशासन प्रकट होता है। साधना अनुशासनपूर्वक अर्थात् नियमित, अखण्ड और निरन्तर करने से ही फलदायी होती है। अतः साधक के हृदय में लक्ष्मी देवी अपने विष्णु शक्ति स्वरूप में आध्यात्मिक साधना में सातत्य तथा नियमितता, इन दो सद्गुणों द्वारा व्यक्त होती हैं, क्योंकि साधक का योगाभ्यास इन दो सद्गुणों पर निर्भर करता है।
लक्ष्मी जी धैर्य तथा संलग्नता-इन दो दैवी सम्पद् के स्वरूपों द्वारा प्रकट होती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे हृदय में उद्भूत निष्कामता तथा आत्म-सन्तोष भी लक्ष्मी देवी के व्यक्त स्वरूप है।
जिस प्रकार गृह-क्षेत्र में बाह्य स्वच्छता आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में शौच का स्थान है। साधक के बाह्य तथा आन्तर जीवन के सभी ओर शुचिता साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है ।
स्वास्थ्य तथा मुदिता, ये दोनों ही देवी के प्रकट स्वरूप हैं।
माता जी की अवहेलना न करें
इसी भाँति अब तक गृह-क्षेत्र में तथा योग और साधना के जीवन-क्षेत्र में माता जी के स्वरूपों के आविर्भाव का वर्णन तथा उसकी आलोचना की गयी। माता जी की दिव्य शक्ति के प्राकट्य के महत्त्वपूर्ण नियम को ध्यान में रखना आवश्यक है। जहाँ माँ लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है, जहाँ उन्हें प्रसन्न किया जाता है, वहीं पर वह निवास करती हैं। जहाँ उनका अनादर होता है, वहाँ वह निवास नहीं करती हैं। इस बात को गृह-क्षेत्र अथवा साधना-जीवन में सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इतना जान लेने पर व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए तथा माता जी की उपेक्षा करने से दूर रहना चाहिए। जिस समय लक्ष्मी माँ के ये स्वरूप विद्यमान हों, उस समय यदि हम उनका सदुपयोग न करें, यदि हम उनकी उपेक्षा करें, तो यह देवी का तिरस्कार करना होगा। वह जैसी अपेक्षा रखती हैं, वैसा सम्मान उन्हें न दे कर हम उनका अपमान करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। अतः यदि व्यक्ति लक्ष्मी की अवहेलना करता है, उनका अनादर करता है, तो भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख-सम्पत्ति उसका त्याग कर जाते हैं।
इस महत्त्वपूर्ण नियम को समझ कर माता जी की, उनके किसी स्वरूप की अवहेलना न करने के लिए हमें सदा सावधान रहना चाहिए। इसी से अपने हिन्दू-घरों में ऐसी मान्यता है कि जब हम भोजन के लिए बैठे हों, उस समय हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय कर्कश शब्द नहीं बोलना चाहिए। भोजन को अस्वीकार करना गम्भीर भूल है। यह पृथ्वी पर जीवन बनाये रखने वाले पोषक तत्त्व-रूप में विद्यमान माता जी का अपमान है, उनकी अवहेलना है। भोजन का अपमान न करें। उसकी उपेक्षा न करें। अतएव जिस हिन्दू-परिवार में यह सत्य समझ में आ गया, वहाँ गृहलक्ष्मी कभी भी भूमि पर चावल बिखरने नहीं देगी; क्योंकि चावल के ऊपर पाँव रखना महादोष है। अन्न लक्ष्मी है। व्यक्ति को अन्न अकारण नहीं फेंकना चाहिए। उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अन्न फेंकने से हम लक्ष्मी देवी के इस स्वरूप की महत्ता तथा अर्हता नहीं समझ सके हैं, ऐसा मानना होगा। निश्चय ही हम अन्नदान करें-गाय, कुत्ता, बिल्ली तथा अन्य भूखे प्राणियों को खिलायें; परन्तु उसे निरर्थक न फेंकें, क्योंकि माता जी स्वयं कृपा कर जब हमारे पास आती हैं, उस समय यदि हम उनका मूल्य नहीं समझते तो ऐसा भी होता है कि जब हमें उनकी अतीव आवश्यकता होती है, तब वह अलभ्य बन जाती हैं।
साधक में लक्ष्मी जी के प्राकट्य का एक और महत्त्वपूर्ण स्वरूप है स्मरण- शक्ति। 'या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता ।' अतः आध्यात्मिक साधक को माता जी के इस स्वरूप को विकसित करने का सदा प्रयास करना चाहिए। देवीसूक्त का कथन है कि माता जी सभी प्राणियों में स्मृति-रूप में विराजती हैं। गुरुदेव के श्रीमुख से निकले उपदेश के अमूल्य तथा उत्कृष्ट शब्दों की, ज्ञान की स्मृति तथा इस लोक के महान् सन्तों तथा भक्तों के जीवन के उदाहरण से तथा उनके वचनों से प्राप्त ज्ञान की स्मृति रूप में माता जी व्यक्त होती हैं। आध्यात्मिक उपदेश के ये रत्न स्मृति द्वारा ही सुरक्षित रखे जाते हैं। यदि हम उन्हें अपने स्मृति-पटल पर स्मरण न रखें, उनका मनन तथा निदिध्यासन न करें, तो हम उन उपदेशों से पूर्णतम लाभ नहीं उठा सकेंगे। यदि माता जी का यह स्मृत्यात्मक स्वरूप हमारे पास न हो, तो हम गुरुदेव के उपदेशों तथा उनकी आज्ञाओं का सन्तोषजनक रूप से पालन नहीं कर सकते। अतः हमें लक्ष्मी देवी के इस महत्त्वपूर्ण स्वरूप की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। 'मुझे स्मरण नहीं है' -इस बहाने से उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि हम गुरुदेव के उपदेशों को स्मरण नहीं रखते, तो अन्त में हमें ही हानि उठानी पड़ेगी।
अतः हम लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करें कि वह हमारे गृह तथा हृदय में विद्या माया के इन दैवी सम्पद् रूपों में प्रकट हों और आशीर्वाद दें। अपने गृह तथा हृदय में विराजमान माता जी के इन स्वरूपों का हम पूर्ण सदुपयोग करें और इस भाँति भावपूर्वक उनका आदर कर पूजन करें। हम उनसे प्रार्थना करें कि हमें इस लोक तथा परलोक में अनन्त कल्याण-लाभ हो।
दिव्य गुरुदेव के पावन चरण-कमलों की शरण लेने का सद्भाग्य जिन शिष्यों और साधकों को इस जीवन में प्राप्त हुआ है, उनसे मैं कुछ विशेष शब्द कहना चाहता हूँ। पवित्र आनन्द-कुटीर में जैसा जीवन-यापन किया जाता है, वैसा दिव्य तथा उदात्त जीवन जीने तथा श्री गुरुदेव के उपदेशानुसार अपना जीवन ढालने के लिए जो साधक प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मैं ये दो शब्द कहता हूँ। इस स्थान में माता लक्ष्मी के सम्पूर्ण प्रकाश तथा सम्पूर्ण महिमा के सर्वाधिक विरल स्वरूप का दर्शन मिलता है। दैवी सम्पद् के सब लक्षण जहाँ प्रचुर मात्रा में सदा निवास करते हैं, ऐसे अनुपम आश्रम के रूप में, ऐसी अद्वितीय संस्था के रूप में वह यहाँ विराजती हैं। यह आश्रम एक अद्वितीय भाग्यशाली तथा मंगलमय स्थान है। हमें यहाँ अत्यन्त दुर्लभ मानव-देह मिलने के पश्चात् मुमुक्षुत्व का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त कर आत्मसाक्षात्कार-प्राप्त महान् सन्त का सतत सान्निध्य-रूपी अनमोल लाभ प्राप्य है। यहाँ पर हमारी साधना के विविध पहलू परिरक्षित रहते हैं और उन्हें दिन-प्रति-दिन विकसित करने के लिए प्रत्येक प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।
भक्तों के लिए मन्दिर हैं, जहाँ उपासना करने का प्रचुर अवसर उपलब्ध है। नाम-जप तथा संकीर्तन के लिए भजन-हाल है, श्रवण-स्मरण आदि नवधा भक्ति के लिए पूर्ण सुविधाएँ हैं तथा मन्दिर के आदर्श वातावरण में अथवा वन में, गंगा के पावन तट पर जप करने की सभी वस्तुएँ उपलब्ध हैं।
वेदान्तियों के लिए उपनिषद् पर नित्य उत्कृष्ट प्रवचन सुनने, श्री स्वामी कृष्णानन्द जी जैसे प्रकाण्ड वेदान्ती के साथ सत्संग करने तथा वन-प्रदेश के एकान्त वातावरण में गम्भीर ध्यान करने के अनेक अवसर सुलभ हैं।
कर्मयोगी के लिए भी ऐसी ही सुविधाएँ हैं। यदि उसे अपने जीवन को साधना में रूपान्तरित करने की, अपने जीवन के अध्यात्मीकरण की सच्ची लगन है, तो उसके लिए यह स्थान साक्षात् स्वर्ग है।
दिव्य गुणों के विकास करने तथा आसन और प्राणायाम की प्रक्रियाओं का अभ्यास करने के लिए यहाँ राजयोगियों के लिए भी श्रेष्ठ सुविधाएँ हैं।
संक्षेप में कहें तो संस्कृत के पण्डित जिसे 'न भूतो न भविष्यति' कहते हैं, ऐसा ही यह स्थान है।
जिस साधना द्वारा सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है, जो ध्येय मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य है, जहाँ पहुँच कर परम सुख प्राप्त होता है, उस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रकार की साधना की सभी प्रकार की सुविधाएँ सुलभ हों, ऐसा विलक्षण स्थान मिलना दुर्लभ है। माता लक्ष्मी जी ने स्वयं गौरवमयी रीति से तथा अबाध कृपा कर इस स्थान को अपने प्राकट्य का स्वरूप बनाया है। यहाँ गंगा माँ, हिमालय, गुरुदेव, गोविन्द की आराधना- ये साधन प्रत्यक्ष वर्तमान हैं। माता लक्ष्मी जी के इस साक्षात् स्वरूप का लाभ उठा कर हम उनका (माता लक्ष्मी का) सम्मान करें, उनकी आराधना करें तथा परम कृपालु परमेश्वर की अहेतुक कृपा से प्राप्त इस अनुपम सुयोग का उपयोग करें-इतना ही करना अब हमारे लिए शेष रहा है।
कुछ समय पूर्व मैंने आप सबका ध्यान आकर्षित किया था कि जिस प्रकार माता जी ने इन रूपों में प्रकट हो कर हमें दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया है, तो हम उनका अनादर करने की भूल न कर बैठें; क्योंकि हम यदि उनकी उपेक्षा करेंगे, तो यह दुर्लभ सुयोग हमारे हाथ से निकल जायेगा। जीवन अनिश्चित है तथा समय तीव्र वेग से भाग रहा है। ऐसे आदर्श वातावरण में मानव-जीवन लाभ का अद्भुत सौभाग्य क्षण मात्र में छिन जायेगा। यदि इसे स्मरण न रखें और देर तक उपेक्षा करते रहें, तो बाद में हमें पश्चात्ताप करना पड़ेगा और इससे हमें अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी। यदि माता जी द्वारा एक बार प्रदत्त इस अमूल्य सुयोग का हम अनादर करेंगे, तो माँ सरलता से पुनः नहीं आयेंगी और ऐसा अवसर पुनः हमें दुष्प्राप्य होगा। जब तक उनकी कृपा-सरिता प्रबल वेग से प्रवाहित हो रही है, तब तक हम सावधान तथा जागरूक रह कर अपनी सत्ता को उस कृपा से आपूरित करने को तत्पर हो जायें तथा धैर्य और संलग्नता से अपनी आध्यात्मिक साधना में लगे रह कर माता लक्ष्मी जी की कृपा तथा सद्गुरुदेव के दिव्य चरण-कमल का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी इहलौकिक जीवन-यात्रा शीघ्र पूर्ण कर नित्य प्रकाश, शाश्वत आनन्द, अमरत्व तथा दैवी पूर्णता के परम धाम में पहुँच जायें।
विद्यास्समस्तास्तव देवि भेदाः
स्त्रिय: समस्ताः सकला जगत्सु ।
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ।।
(दुर्गासप्तशती ११-६)
हे देवी! विद्याएँ सारी भेद आपका कहलाती।
जग की स्त्री मात्र सभी प्रतिबिम्ब आपका दर्शार्ती ।।
हे अम्बे! यह जग पूरित है सारा आपकी महिमा से।
मैं क्या स्तुति करूँ, परे हो, पर स्तुति की गरिमा से ।।
सप्तम रात्रि
ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः
सृष्टि माता की वीणा का संगीत
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ।।'
धवल तुषार कुन्द चन्दा-सा हार शुभ्र वस्त्रों वाली।
जो कर में वीणा वर धारे श्वेत पद्म आसन वाली ॥
जो ब्रह्मा शिव विष्णु सदृश देवों से नित वन्दित हैं माँ।
बुद्धि की जड़ता हर, वह ही रक्षा करें सरस्वती माँ ।।
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय की आधारभूता ब्रह्ममयी महिमान्विता माँ को हमारा भक्तिपूर्ण प्रणाम! ज्ञानदायिनी, समस्त प्रपंच की रचयित्री व ध्वंसकारिणी तथा सम्पूर्ण ज्ञान की पूर्णता और चरम परिणतिरूपा माँ को बार-बार प्रणाम! उनकी कृपा हम सब पर हो!
आज हम सब परमात्मा की पराशक्ति महासरस्वती की पूजा हेतु भक्तिपूर्ण हृदय से यहाँ आये हैं। महासरस्वती शुद्ध शब्द-रूप में अति-प्राकृत आविर्भाव हैं। महासरस्वती सृष्टि के क्रमिक विकास की, जीव तथा उसके प्रपंच की उत्पत्ति से लय पर्यन्त समस्त क्रिया की पूर्ण मूर्ति हैं। वही ब्रह्मा-शक्ति के रूप में महाशक्ति हैं और सृष्टि-क्रिया के आरम्भ से कार्य करती हैं। माता जी मन तथा इन्द्रियों से अगम्य एवं नाम-रूप-रहित जो परम तत्त्व है, उसमें से प्रकट होने वाले समस्त नाम-रूपों के प्राकट्य तथा प्रक्षेपण की अधिष्ठात्री हैं। इस स्थिति में वह समस्त जीवन-प्रक्रिया के मूल में रहती हैं। उस अखण्ड एकरस सच्चिदानन्द परब्रह्म से सृष्टि-धारा प्रवाहित हो कर क्रमशः स्थूल से स्थूलतर रूप में अवतरित हो कोटि-कोटि नाम-रूपों के परिणाम को प्राप्त होती है और महामाया के साम्राज्य में भ्रामक विश्व-नाटक के रूप में प्रकट होती है। उस समय माता सरस्वती यवनिका के पीछे चली जाती हैं और इस नाटक को आगे चलाने के लिए अपने अन्य दो स्वरूपों-विष्णुमाया तथा दुर्गा देवी के हाथों में छोड़ देती हैं। परन्तु जब परब्रह्म की कृपा से जीव के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया आरम्भ होती है, तब विकास-चक्र की प्रक्रिया की पूर्णाहुति प्रारम्भ होती है। जीव पुनः आन्तरिक योग-मार्ग से ऊपर चढ़ना आरम्भ करता है तथा अन्दर वर्तमान चेतन तत्त्व की स्थूलता को क्रमिक रूप से हटाता हुआ वह सत्त्व, दैवी सम्पद् तथा आध्यात्मिकता के पथ में आगे बढ़ते-बढ़ते योग के सर्वोत्कृष्ट शिखर तक पहुँच जाता है। इस समय माता जी जीव में महासरस्वती रूप में, उसकी अन्तश्चेतना में आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान रूप में प्रकट होती हैं। इस भाँति माता जी जीव के विवर्तन-चक्र को शेष करती हैं तथा जीवात्मा एक बार पुनः परब्रह्म में विलय होता है। इस प्रकार माता सरस्वती सर्जन-शक्ति के रूप में नाम-रूप-रहित परब्रह्म से होने वाली इस विकास-प्रक्रिया के मूल में हैं। एक से अनेक की सृष्टि करने वाली माता जी परम ज्ञानदायिनी रूप में अन्तिम समय विशुद्ध ज्ञान-स्वरूप में प्रकट होती हैं। वह इस संसार-चक्र का आवर्तन पूर्ण करती हैं। इसी से हम उनमें इस संसार-सृष्टि की क्रीड़ा की पूर्णता देखते हैं। माता जी की इन उभय स्वरूपों में पूजा की जाती है। साधक, भक्त तथा योगी के लिए माता जी का यह स्वरूप बहुत ही महत्त्व का है; क्योंकि उसे कैवल्य मोक्षप्रदायक ज्ञान माता सरस्वती ही प्रदान करती हैं।
योग के तत्त्व तथा उसकी क्रिया
हम माता जी की जो मूर्ति देखते हैं, उससे हमें सरस्वती माता की दो परमोच्च क्रियाओं का विचार आता है। उनके एक हाथ में वीणा है, जिसका विचार हम अभी करेंगे और उनके अपर हाथों में सुन्दर स्फटिक माला तथा वेद-ग्रन्थ हैं। उनके हाथ में पुस्तक है। पुस्तक तथा माला हाथ में ग्रहण करने का भाव यह है कि परा तथा अपरा तत्त्व का समस्त ज्ञान उनके करतलगत है। सृष्टि के सम्पूर्ण पदार्थों का पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण सृष्टि के आदि-रूप परब्रह्म के परा ज्ञान का जिनमें विस्तृत वर्णन है, उन सब वेदों को वह अपने हाथ में रखती हैं; क्योंकि वेद जिसमें से प्रथम प्रकट हुए उस ब्रह्मा की वह क्रिया-शक्ति हैं। ब्रह्मा वेद-पिता तथा वेद-दाता हैं। माता सरस्वती स्वयं ब्रह्मा की, चतुर्मुख ब्रह्मा की शक्ति हैं। ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रतिनिधि तथा परम, मूल भण्डार रूप हैं तथा माँ सरस्वती वैदिक ज्ञान की प्रकट स्वरूप हैं। इसी से माता जी ब्रह्मज्ञान के तत्त्वों को समाविष्ट करने वाले वेद-ग्रन्थ को अपने हाथ में धारण किये हैं। आत्म-साक्षात्कार के पथ में वेद-ग्रन्थों के पाठ तथा गुरु के श्रीमुख से प्राप्त सत्य के सिद्धान्तों के ज्ञान को अभ्यास तथा निदिध्यासन द्वारा स्वानुभूति में रूपान्तरित करना होता है। यह योगाभ्यास जिसके द्वारा वेद का सत्य उपलब्ध होता है, उसका प्रतीक माँ के दाहिने हाथ की शुद्ध स्फटिक माला है। माला योगाभ्यास के कार्यान्वयन की सूचक है। वेद की ज्ञान-शक्ति एवं योग तथा आध्यात्मिक साधना की क्रिया-शक्ति- ये दोनों मिल कर माँ का पूर्ण रूप हैं।
माँ विशुद्ध सत्त्व हैं
माता जी का चित्रण शुभ्र विशुद्ध वसन से परिवेष्टित एवं निष्कलंक निर्दोष सौन्दर्य की पराकाष्ठा के रूप में किया गया है। माता जी की धवलता की कुन्द-पुष्प, चन्द्रमा तथा हिमालय की चिर अनधिगम्य तुषार-माला के निष्कलंक सौन्दर्य से तुलना की गयी है-"या कुन्देन्दुतुषारहारधवला।" कुन्द का अर्थ है कुमुदिनी, इन्दु चन्द्रमा को कहते हैं तथा तुषारहार का अर्थ है-हिम-श्रृंखला। विश्व की इन तीन सर्वोत्कृष्ट, निर्मल तथा धवल वस्तुओं से उनकी समता की जाती है। वह विशुद्ध श्वेत वस्त्र से परिहित हैं, ऐसा वर्णन यह बतलाने के लिए किया गया है कि माता जी अनून विशुद्ध सत्त्व की घनीभूत रूप हैं; क्योंकि वह परब्रह्म का प्रथम आविर्भाव हैं।
माता सर्वरूप हैं
हम जानते हैं कि वेद के अनुसार अव्यक्त निराकार निर्गुण परब्रह्म के हृदय में से सर्वप्रथम प्रणव का प्राकट्य हुआ। अज्ञेय तुरीय सत्ता के प्रथम शुद्ध संकल्प के समय जो प्रथम स्पन्दन अथवा अलौकिक कम्पन हुआ, उसे वेद 'एकोऽहं बहुस्याम् प्रजायेय' - 'मैं एक हूँ अनेक बनूँ', ऐसा कह कर वर्णन करते हैं। इस लाक्षणिक कथन का कारण यह है कि जो एक था, वह दृश्य रूप से अनेक किस प्रकार बना, इसे हम समझ सकें। उसका प्रथम शुद्ध संकल्प इस प्रकार स्पन्द-रूप से आविर्भूत हो प्रथम तथा आद्य व अतीन्द्रिय शब्द अथवा नाद-रूप से व्यक्त हुआ। इसे ही हम सब प्रणव-रूप में जानते हैं। यह नाद ब्रह्म अथवा प्रणव माता सरस्वती का ही रूप है। माँ सरस्वती प्रणवरूपिणी हैं। माँ सरस्वती में नाद-ब्रह्म तथा शब्द-ब्रह्म, ये दो स्वरूप समाहित हैं। नाद प्रणव है और शब्द उसकी मूल ध्वनि का स्वरूप है। यह प्रणव जब व्यक्त तथा उच्चारित होता है, तब वह वाणी के क्षेत्र में प्रकट होता है। प्रथम शब्द वाणी बनता है। इसी से माता जी वीणा तथा वाणी कही जाती हैं। उनके हाथ में इस विशुद्ध शब्द को प्रकट करने का यन्त्र वीणा है एवं वह सब उच्चारित नामों की जननी हैं। अतः इस रूप में वह 'वाणी' हैं। इस वीणा की ध्वनि के मध्य में ही सम्पूर्ण वेद-मन्त्रों की उत्पत्ति का स्थान है। इस विषय में अधिक गम्भीरता से उतरने पर हम पाते हैं कि यह अखिल विश्व परमा माँ की वीणा की झनकार ही है, इसके अतिरिक्त वह अन्य कुछ भी नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत्, यह समस्त सृष्टि माँ सरस्वती की वीणा से निःसृत सनातन संगीत के स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है; क्योंकि हम जानते हैं कि यह दृश्य जगत् रूप अथवा आकार से निर्मित है। जो कुछ भी हम इन्द्रियों द्वारा देखते, स्पर्श करते अथवा अनुभव करते हैं, वह सब रूप का ही स्वरूप है। यह जगत् अपने रूप के द्वारा ही हमारे सम्मुख प्रकट होता है और प्रत्येक रूप का एक विशेष नाम है। विश्व में जो असंख्य रूप हैं, वे अपने असंख्य नामों द्वारा ही हमें बोधगम्य होते हैं। ये नाम अमुक अक्षरों के संयोजन हैं। ये अक्षर जो असंख्य भिन्न-भिन्न नाम गठित करते हैं, वे ध्वनि के उच्चारित रूप हैं। स्फुटित ध्वनि अक्षर-रूप में प्रकट होती है और ये रहस्यमय अक्षर संयोजित हो कर नाम का गठन करते हैं, जिसका अर्थ रूप के आकार में प्रादुर्भूत होता है। यही दृश्य जगत् है। प्रत्येक अक्षर जिस नाद का स्फुट स्वरूप है, वह नाद अन्ततः तात्त्विक रूप में विशुद्ध स्पन्दन है और यह स्पन्दन माता जी की वीणा के संगीत से उत्पन्न होता है।
इस भाँति सरस्वती की वीणा के दिव्य तारों की झनकार के स्पन्दन से नाद प्रकट होता है। यह नाद जब प्रस्फुटित होता है, तब अमुक अक्षर बन कर नाम का निर्माण करता है और ये नाम अपना अर्थ प्रकट करने वाले अगणित रूपों में व्यक्त होते हैं, जिसे जगत् कहते हैं। इसलिए यह समस्त दृश्यमान् जगत्, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और यह ब्रह्माण्ड ही क्यों सर्वातीत सत्ता से उद्भूत तथा प्रत्येक क्षण उत्पन्न हो रहे असंख्य संसार माता की वीणा के संगीत की बाह्य अभिव्यक्तियाँ हैं। इस संगीत की सूत्रधार-शक्ति सरस्वती जी हैं। वह परम शुद्ध सत्त्व हैं तथा अन्तिम तत्त्व हैं, जिनके चिन्तन से ही हम शीघ्र ही शुद्ध तुरीय अवस्था में, परम सत्ता में पहुँच जाते हैं। हमारे लिए माता सरस्वती का यही स्वरूप है। उनकी वीणा ओंकाररूपा है तथा यह विश्व उनकी वीणा द्वारा व्यक्त शुद्ध दिव्य नाद के रूप में अभिव्यक्त उनकी ही शक्ति है।
जिस दिव्य ज्योति के प्रकाश से अन्धकार दूर होता है
सप्तशती में हम देखते हैं कि महिषासुर के निधन के समय माँ रूद्र-रूप में उसके समक्ष प्रकट हुई थीं। यह विलक्षण तथा समझने योग्य बात है। जब महासरस्वती-रूप में माँ समस्त प्रपंच के सृजन की मूल कारण हैं, तो रणभूमि में रुद्र-रूप में उनके आविर्भाव होने का कारण क्या है? शुद्ध सर्जक शक्ति कभी ध्वंस किस प्रकार कर सकती है? किन्तु यदि हम सृष्टि-चक्र के दूसरे छोर पर व्यक्त होने तथा चक्र के पूर्ण होने पर शुद्ध ब्रह्मज्ञान में परिणत होने वाले माता जी के स्वरूप पर जरा विचार करें, तो यह शंका तुरन्त दूर हो जायेगी; क्योंकि माता जी वस्तुतः विनाश नहीं करतीं, अपितु जिस क्षण जीवात्मा उनके सान्निध्य में जाता है और जिस क्षण वह अपने उज्ज्वल आलोक से उद्भासित हो प्रकट होती हैं, उसी समय उसके जन्म-मृत्यु-रूप चक्र की गति समाप्त हो जाती है। इसी से उनके प्राकट्य मात्र से संसार-रोग का आशु नाश होता है। उनके महिमामय आविर्भाव से मृत्यु भी मृत्यु को प्राप्त होती है और अज्ञानान्धकार समूल नष्ट हो जाता है। अतः उन्हें वस्तुतः किसी का विनाश करना नहीं होता। उनके आविर्भाव मात्र से अज्ञान-रूपी अन्धकार स्वयमेव नष्ट हो जाता है, संसार-चक्र की गति निरुद्ध हो जाती है। माता जी जीव में रहे जड़त्व के अन्तिम अवशेष को भी सदा के लिए उत्पाटित कर डालती हैं। उस समय शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के साथ जीव का अभेद हो जाता है।
जीव के चैतन्य क्षेत्र में महासरस्वती के रूप में माँ के आविर्भाव होने मात्र से अज्ञानान्धकार का अचिर ध्वंस होता है, जड़त्व नष्ट हो जाता है, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है तथा 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणं' का प्रवाह समाप्त हो जाता है। माँ के प्राकट्य से जीव पूर्ण ब्रह्मज्ञान लाभ करता है।
इस भाँति माता जी की उपासना का बहुत ही सुन्दर लाक्षणिक अर्थ है। हमारी उपासना में आत्यन्तिक मोक्ष-प्रदायिका शक्ति की ही आराधना है, ऐसी बात नहीं है। यह युगपत् विराट् की भी उपासना है; क्योंकि हम जब माँ की महासरस्वती के रूप में उपासना करते हैं, तो हम अखिल विश्व की उपासना करते हैं। हम देख चुके हैं कि समस्त जगत् और कुछ नहीं है। वह अपनी प्रथमावस्था में दिव्य नाद रूप में प्रकटित उनकी पराशक्ति का आविर्भाव तथा साक्षात् स्वरूप है। हम जो कुछ भी देखते हैं, वह सब माता सरस्वती की शक्ति का ही घनीभूत रूप है। हम जो माँ की पूजा करते हैं, उसमें केवल परम पुरुष के मातृ-स्वरूप की पूजा है, ऐसा नहीं है। वह विश्व-रूप भगवान् की पूजा है। इसके साथ ही पराशक्ति के उस स्वरूप की भी पूजा होती है, जिसकी कृपा से ही हम अज्ञान-रूपी अन्धकार के पंजों से छुटकारा पाते हैं और अमरता, असीम ज्ञान तथा अनन्त आनन्द के परम धाम में पहुँचते हैं।
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।।'
(दुर्गासप्तशती : ५-८०)
कर पूरा जग व्याप्त है स्थित जो चैतन्य स्वरूपा माँ।
नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है उसे नमः ॥
अष्टम रात्रि
ॐ प्राणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु
सिद्धि तथा सफलता की देवी
जय सरस्वति जय सरस्वति जय सरस्वति पाहि माम्।
श्री सरस्वति श्री सरस्वति श्री सरस्वति रक्ष माम् ॥
जो प्राणों की अधिष्ठातृ माँ सरस्वती कहलाती।
इन्द्रिय का इन्द्रिय के द्वारा ही नेतृत्व है करवाती ।।
और बुद्धि की रक्षा, संरक्षण को माता करवाती ।
सबकी रक्षा करें वही माँ जो सरस्वती कहलाती ॥
इस सम्पूर्ण जगत् की स्थिति तथा शेषरूपा भगवती जननी ! तुम्हें नमस्कार। सर्वातीत सत्य की अचिन्त्य अनिर्वचनीय शक्तिस्वरूपा ब्रह्मरूपिणी माँ को प्रणाम। जो महाशक्ति, आद्यशक्ति, पराशक्ति सरस्वती स्वरूप में प्रकट हो, हमें परब्रह्म का परम ज्ञान प्रदान कर दुःख और मृत्यु के मायिक जीवन से मुक्त करती हैं, ऐसी जगदम्बा को मेरा बार-बार प्रणाम।
समस्त दृश्य जगत्, प्रपंच तथा मानव-दृष्टि से परे अवस्थित अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-ये सब माँ सरस्वती के अलौकिक तथा भव्य प्रकट रूप हैं। वही बुद्धि से अगम्य परब्रह्म की शक्ति की आद्य स्वरूप हैं। वही रहस्यमय नाद के रूप में सर्वप्रथम प्रकट होती हैं। इसी से वह नादरूपिणी सरस्वती के रूप में पूजित हैं। वह परम श्रेष्ठ प्रणवरूपा हैं, इसी से वह चिद्रूपिणी अथवा शब्दरूपिणी भी कहलाती हैं। परब्रह्म चिद्रूप है। वह निश्चल तथा निष्क्रिय है। उसमें किसी प्रकार की गति अथवा कम्पन नहीं है। वह निस्पन्द है। वहाँ न तो ध्वनि है, न क्रिया है और न गति ही है। वह अशब्द, निस्पन्द तथा निष्क्रिय है।
इस अनन्त आनन्दघन का प्रथम स्पन्दन बिन्दु के रूप में क्योंकर प्रकट हुआ, इसका वर्णन वेदों में किया गया है। ज्ञानघन के मध्य में उद्वेलन से आविर्भाव ही यह अलौकिक बिन्दु है, सभी वर्तमान पदार्थों का कारण है। यह बिन्दु नाद-रूप में प्रकट होता है। असीम चिद्दन में उत्पन्न हुआ आदि स्पन्दन बिन्दु-रूप में प्रकट होता है। उसका प्रकाश नाद है और वही माँ सरस्वती हैं। हम देख चुके हैं कि इसी से माता सरस्वती की कल्पना शुद्ध, विमल, श्वेतवसना, अवर्णा तथा सम्पूर्ण नाद-शक्ति की प्रतिमूर्तिरूपा वीणाधारिणी के रूप में की गयी है। आदि शब्द नाद से शुद्ध ध्वनि के रूप में क्रमशः सम्पूर्ण वैखरी शब्द-राशि की सृष्टि होती है। वैखरी शब्द ही वाक् है। वाक् का प्रकटीकरण वर्ण अथवा अक्षर-रूप में होता है। वर्णों के संयोजन से शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द ही नाम है। नाम के साथ ही उसके अर्थज्ञापक रूप का आविर्भाव होता है। हम इस दृश्य जगत् में जो कुछ भी देखते हैं, वह सब नामरूपात्मक है। यह दृश्य जगत्, जो कि अनन्त रूप है, माता सरस्वती अथवा आदि शब्द ब्रह्म का ही अन्तिम परिणाम है, जिसका प्रथम ध्वनि-रूप में, तदनन्तर क्रमशः वाक्, वर्ण तथा नाम और अन्त में आकार-रूप में आविर्भाव हुआ।
यह सृष्टि जो मनुष्य तथा पदार्थ के रूप में विकसित है, उस आदि परम सत्य की ही विशेष अभिव्यक्ति है। आज हम इस पर ही विचार करेंगे। पिछले दिनों में हमने माँ का नाम-रूप की शक्तिमयी ध्वंसकारिणी दुर्गा देवी के रूप में तथा त्रिकाल में नाम-रूप की रक्षाकारिणी-पालनकर्ती लक्ष्मी के रूप में पूजन किया था। उस समय हमने उनके केवल मूल प्रापंचिक स्वरूप का ही वर्णन नहीं किया था, अपितु मनुष्य और उसके व्यावहारिक जगत् के क्रियाकलापों में माता जी किन-किन स्वरूपों में व्यक्त होती हैं, इसका भी निरूपण किया था। इसके साथ ही जीव के पूर्णता प्राप्ति के लक्ष्य तथा परब्रह्म से उसके मिलन के लिए व्यवहृत होने वाले आन्तरिक योग-मार्ग में साहाय्य करने के लिए माता जी साधक की आन्तर चेतना तथा व्यक्तित्व में किस प्रकार प्रकट होती हैं, इसका भी हमने विचार किया था।
जब हम इस विषय-जगत् में माता जी के स्वरूपों का विचार करते हैं, तो देखते हैं कि मनुष्य के व्यवहार-जगत् में जितना पराशक्ति का दुर्गा माता तथा लक्ष्मी माता के रूप में प्रकटीकरण हुआ प्रतीत होता है, उतना माता सरस्वती के रूप में प्राकट्य नहीं अनुभव होता। इसका एकमात्र कारण यह है कि दृश्य जगत् में प्राकट्य तथा सृष्टि के मूल उद्गमस्थान-रूपी स्रोत की ओर प्रत्यावर्तन के विकास-प्रक्रिया-चक्र के उभय छोरों पर उनका अधिष्ठान माना गया है। हम देख चुके हैं कि सर्जन-प्रणोद के रूप में माता जी क्या कार्य करती हैं। ब्रह्म का अव्यक्त शक्ति-तत्त्व जब विश्व में प्रकट होता है, तब उसके ऊपर सरस्वती माँ का आधिपत्य माना जाता है। इस भाँति विश्व-कार्य में माँ सरस्वती का कार्य प्राथमिक है।
विश्व की रचना कर माँ (सरस्वती) यवनिका के पीछे पार्श्वभूमि में चली जाती हैं। पदार्थों के एक बार प्रकट हो जाने पर तथा जो अनामी था, उसके नाम-रूप धारण कर लेने पर वह (सरस्वती) प्रतिसरण कर जाती हैं और अगली प्रक्रिया को लक्ष्मी देवी तथा दुर्गा देवी के रूप में प्रकट अपने अन्य दो स्वरूपों को हस्तान्तरित कर देती हैं। इसी से हम माता जी के संरक्षक स्वरूप लक्ष्मी देवी से अधिक अवगत हैं। उनका कार्यक्षेत्र दीर्घ काल तक विस्तृत होने से हमें वह सतत प्रवर्तमान प्रक्रिया-सा लगता है। इसी से शक्ति के उस स्वरूप की क्रीड़ा के ऊपर हमारा ध्यान अधिक केन्द्रित होता है।
इसी भाँति समस्त नाम-रूपों को निर्विकार भाव से विलय करने वाली दुर्गा माता जी की अन्तिम लीला के ऊपर भी हमारा ध्यान केन्द्रित होना स्वाभाविक ही है। मनुष्य के मन तथा आन्तर चेतना में इन दोनों के प्रति ममत्व होने का एक बहुत ही सहज तथा बोधगम्य कारण है और वह यह है कि नाम तथा रूप के प्रति, विश्व की प्रत्येक वस्तु के प्रति मनुष्य की ममता तथा तज्जन्य आसक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह इन नाम-रूपों तथा वस्तुओं के पोषण में तथा उनका अस्तित्व सदा बनाये रखने के प्रयत्न में मग्न रहता है। इससे जब उन नाम-रूपों तथा वस्तुओं का विनाश होता है, तब वह स्तब्ध-सा रह जाता है, उसे गहरा आघात पहुँचता है। ममता के परिणाम-स्वरूप दृढ़ बनी आसक्ति के कारण व्यक्ति विनाश अथवा मृत्यु की बात पसन्द नहीं करता। उसके हृदय में दुःख होता है। इसके परिणाम-स्वरूप उसके मन में इस विनाश-प्रक्रिया का आतंक छाया रहता है। उसके मन में इस बात की स्मृति सतत बनी रहती है और उसे इससे भय लगता है। अतः यह विचार उसके मन को घेरे रहता है। जिन वस्तुओं को वह 'मेरी' समझता है, उनमें उसका ममत्व होता है। उन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए वह माता लक्ष्मी के कार्य में सहायता करता है। परन्तु सरस्वती देवी में से होने वाला सर्जन अथवा सृष्टि का प्राकट्य उसे सहज लगता है और एक बार प्रकट हो गया, तो मनुष्य का ध्यान उस ओर नहीं जाता। यही कारण है कि व्यक्ति को सरस्वती-तत्त्व के रूप में माता की विद्यमानता प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होती। परन्तु तर्क द्वारा भी यह जाना जा सकता है कि माता जी के सरस्वती-स्वरूप का भी अस्तित्व अपरिहार्य-रूप में है; क्योंकि यदि सृष्टि न हो, तो अनुराग के लिए वस्तुओं का अस्तित्व ही क्योंकर होता? इस भाँति प्रत्येक वस्तु की स्वाभाविकता देखते हुए प्रत्येक विद्यमान वस्तु के अस्तित्व के लिए सरस्वती माँ एक अपरिहार्य तत्त्व हैं, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा।
सफलता का रहस्य
माँ सृष्टि-प्रक्रिया का केवल प्रवाह ही नहीं हैं; अपितु उनका आदि भी हैं; क्योंकि आदि से ही सृष्टि का प्रारम्भ होता है। इसी से हिन्दू-समाज में माँ की आरम्भ-रूप में भी पूजा की जाती है। जो भी कार्य आरम्भ होता है, वह माता सरस्वती की कृपा से ही होता है, ऐसी मान्यता है। यह एक विचित्र-सी बात है कि सभी आरम्भों की अधिष्ठातृ देवी माँ सरस्वती के साथ-ही-साथ प्रत्येक श्रद्धालु हिन्दू ईश्वर के एक विशेष स्वरूप का गणपति के रूप में पूजन करता है। गणपति भी आरम्भ का एक स्वरूप-नकारात्मक स्वरूप है। गणपति को भी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जब कि माता सरस्वती बुद्धि के क्रियात्मक स्वरूप का प्रतीक मानी जाती हैं। सरस्वती के पूजन से गणपति-पूजन अधिक लोकप्रिय है जो विघ्नों के निवारणार्थ किया जाता है, जब कि माता सरस्वती के पूजन का केन्द्रीय उद्देश्य सदा यह रहता है कि वह सभी प्रारम्भ किये हुए कार्यों को अपनी कृपा द्वारा सफलता प्रदान करें। आइए, अब विचार करें कि अपने इस स्वरूप में माता जी मानव-सृष्टि में किस प्रकार प्रकट होती है। उदाहरण-स्वरूप परसों एक ऐसा प्रसंग आने वाला है, जब माता जी की सर्वारम्भ की अधिष्ठातृ देवी के रूप में पूजा की जायेगी। पवित्र परम्परा के अनुसार यह विजयादशमी का दिन विद्यारम्भ के लिए निर्धारित है। कला अथवा विज्ञान के अभ्यास के आरम्भ के लिए विजयादशमी को अतीव मांगलिक दिवस माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आरम्भ किया हुआ कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। संगीत के समस्त वाद्यों का, रचनात्मक कला से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु का तथा मानव के सामाजिक जीवन की इन सृजनात्मक प्रक्रियाओं से सम्बद्ध सभी पदार्थों का इस विजयादशमी के दिन पूजन किया जाता है। जगत् के व्यक्त स्वरूप अक्षरों को ग्रन्थ-रूप में सुसज्जित कर रूढ़िगत रीति से नवमी के दिन पूजा की जाती है और दशमी के दिन योग्य मुहूर्त में इन ग्रन्थों को पूजा-गृह से बाहर निकाला जाता है और विद्यारम्भ किया जाता है।
यह सब मनुष्य की बाह्य प्रकृति के ऊपर होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि विशेषकर इस आश्रम में आध्यात्मिक जीवन का प्रारम्भ भी इस मांगलिक दिवस को दीक्षा से ही होता है। आप सब जानते हैं कि रहस्यमय नाद वाक् तथा वर्ण का रूप धारण करता है। हमारे मन्त्र इन वर्णों के गूढ़ संयोजन हैं। मन्त्र सरस्वती के स्थान-सीमित शक्ति के पुंजीभूत रूप हैं। इन मन्त्रों का जप सच्चे साधक को बीजातीत ज्ञान प्रदान करता है। सभी साधकों को सरस्वती के इस स्वरूप का ज्ञान 'मन्त्र-उपदेश' के रूप में दिया जाता है। साधक के आन्तर आध्यात्मिक विकास के प्रारम्भ का यह प्रस्थान-बिन्दु भी है। माता जी वैदिक ज्ञान के प्रतीक रूप में एक हाथ में पुस्तक धारण किये हैं और उस ज्ञान के आचरण के लिए दूसरे हाथ में शुद्ध स्फटिक माला धारण किये हुए हैं।
यदि हम इस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इस विश्व में मानव जाति के विशाल जीवन में माता सरस्वती के रूप में पराशक्ति की लीलाओं पर दृष्टिपात करें, तो हम देखेंगे कि इस विश्व में जो भी सृष्टि-कार्य चल रहा है, उसका मूल-तत्त्व माता सरस्वती ही हैं। इसी से अपने यहाँ तथा विज्ञान में प्रगत पाश्चात्य देशों में किये जाने वाले शोध-कार्य, इन वैज्ञानिक शोधों के परिणाम-स्वरूप हुए आविष्कार, वैज्ञानिक नियमों के अन्वेषण से किये गये अनुसन्धान तथा इन अनुसन्धानों का प्रयोग भगवती माता सरस्वती की ही लीलाएँ हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार, अन्वेषण तथा ऐसे आविष्कारों पर आधारित विविध साधित्रों का निर्माण- ये सब माता सरस्वती के प्रकट स्वरूप हैं।
हम पहले कह चुके हैं कि माता जी सभी प्रारम्भों में रहती हैं। अतः दिवस के शुभ प्रारम्भ में भी वह आध्यात्मिक बिन्दु-रूप में रहती हैं अर्थात् जब रात्रि के चार प्रहर समाप्त हो जाते हैं और रात्रि व्यतीत हो जाती है तथा नवीन दिवस का शुभारम्भ होता है, उस समय पवित्र ब्राह्ममुहूर्त की शान्त गम्भीर वेला में माता अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में पूर्ण रूप से प्रकट होती हैं। वह वेला ज्ञानदायिनी माता सरस्वती की अध्यात्मकारी शक्ति से व्याप्त होती है। इसी कारण से नूतन वर्ष भी मंगलमय माना जाता है। वह सरस्वती-रूपा दिव्य शक्ति की अध्यात्मकारी शक्ति से परिव्याप्त रहता है। माता जी की भावमयी आराधना के साथ यदि कोई नया व्यवसाय उस दिन आरम्भ किया जाये, तो वह अपनी पूर्ण कृपा की वृष्टि कर उसमें सफलता प्रदान करती हैं। कोई भी नया अध्यवसाय अथवा नवीन संस्था की स्थापना माता सरस्वती की कृपा से ही शक्य बनता है। यह भी माता सरस्वती के आविर्भाव का एक स्वरूप है। विशेषकर यहाँ आनन्द-कुटीर में कोई शुभ कार्य प्रारम्भ करना होता है, तो सर्वप्रथम माता की पूजा तथा उनके आशीर्वाद की याचना की जाती है। उदाहरण-स्वरूप निर्माण के लिए किसी कार्य में नींव खोदने, शिलारोपण करने के पूर्व माता सरस्वती की आराधना की जाती है।
इसी भाँति सभी व्यापार तथा व्यवहार माता सरस्वती की पूजा तथा भक्तिभावपूर्ण आराधना के रूप में करना होता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, दक्षिण भारत के सभी व्यापारिक केन्द्रों में इस प्रथा का आचरण किया जाता है। महाराष्ट्र में इस व्यापार के फल-स्वरूप उत्पन्न हुई लक्ष्मी के ऊपर ही सबका ध्यान केन्द्रित दिखायी पड़ता है। वहाँ व्यापारी-वर्ग के लोग सरस्वती की अपेक्षा सम्पत्ति की देवी लक्ष्मी के उपासक अधिक हैं। चाहे किसी प्रकार से आराधना करें, अन्त में आराधना तो परब्रह्म की ही होती है। परन्तु हमें यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य की सब प्रकार की प्रवृत्तियाँ पराशक्ति के विविध स्वरूप की लीलाएँ, ही हैं-चाहे वह लक्ष्मी-स्वरूप की, दुर्गा-स्वरूप की अथवा सरस्वती-स्वरूप की हों। इसे ध्यान में रख कर सभी प्रवृत्तियों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनायें तथा पराशक्ति माता की भक्ति-भाव से, उनकी पूजा की भावना से व्यवहार की सभी क्रियाओं का आचरण करें, तो हम अपने व्यवहार-जगत् के कार्यों का भी अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए उपयोग कर सकेंगे। यदि इतना किया गया, तो सांसारिक मनुष्य को इस परिवाद का अवसर नहीं आयेगा कि उसे पूजा, ध्यान तथा योग-साधना का समय अथवा अवसर नहीं मिलता है। जो व्यक्ति सभी प्रवृत्तियों के आध्यात्मिक स्वरूप तथा उनके पीछे पराशक्ति के सूत्रधार हाथों को देख नहीं पाता है, वही ऐसा परिवाद करता है।
इसी के कारण ही मनुष्य सोचता है कि उससे आध्यात्मिक साधना नहीं हो सकती और उसे आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त होने की कोई शक्यता नहीं है। यह बहुत बड़ी भूल है; क्योंकि श्रद्धालु हिन्दू तथा भारतीय प्रतिभावान् व्यक्ति की ऐसी दृढ़ भावना होती है कि उसका सम्पूर्ण जीवन परमात्मा के प्राप्त्यर्थ है, आत्म-साक्षात्कार के लिए है। श्रद्धालु हिन्दू के लिए जीवन का इतना ही मूल्य है कि जीवन जीवात्मा को त्वरित विकास कर मानव-जीवन के चरम लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार हेतु प्राप्त एक सुअवसर है। उसके लिए जीवन का इससे अधिक कोई महत्त्व नहीं है। अतः हमें ऐसा जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। हिन्दू के लिए कोई भी व्यवहार लौकिक नहीं है। समस्त गतियाँ भगवती माँ की व्यक्त स्वरूप हैं और सभी प्रवृत्तियाँ पराशक्ति की सतत पूजा-रूप ही हैं, ऐसा दृष्टिकोण रख कर हमें अपनी प्रवृत्तियों के प्रति अपने समस्त भाव बदलने होंगे। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम तो व्यवहार में उलझे हुए हैं, पतित हैं, आध्यात्मिक सत्य से बहुत दूर हैं। साधना के लिए अवसर के अभाव का खेद करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत सभी कार्य आनन्द-भाव से करने चाहिए, उत्साह से, प्रफुल्लित तथा विकसित मन से करने चाहिए; क्योंकि हमें यह जान लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं, वह मातृ-पूजा ही है। इसी से हम जो कुछ भी करते हैं, उसे पूजा-भाव से करना चाहिए। हमें यह ज्ञात होगा कि मनुष्य को अपना व्यवसाय अथवा स्थान-परिवर्तन करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है और न परम्परागत निवृत्ति-मार्ग के लिए आवश्यक एकान्तिक जीवन-यापन हेतु अरण्य में पलायन करने की ही आवश्यकता है। यदि ऐसा अवसर आये कि आप एकान्त तथा ध्यान में समय व्यतीत कर सकें, तो यह अत्युत्तम है; किन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो सके, जैसा कि सामान्य मानव-समुदाय के जीवन में होता है, तो खेद करने का कोई कारण नहीं है; क्योंकि यदि पदार्थों के प्रति एक बार यथोचित दृष्टि स्वीकार की गयी और उनके प्रति सम्यक् भाव अपनाया गया, तो हम जो कुछ भी करते हैं वह अपरोक्ष रीति से 'योग' तथा 'आध्यात्मिक साधना' ही है। नवरात्र के नौ दिवस की माता जी की आराधना से यह सत्य सविशेष स्पष्ट होता है। हाथ काम करता है, नेत्र देखते हैं, नासिका सूँघती है, कान सुनते हैं तथा जिह्वा बोलती है- ये सभी क्रियाएँ माता जी के गतिशील स्वरूप की पूजा ही हैं। इस बात की स्मृति दिलाने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने भगवती माता की नवरात्र-पूजा का अपूर्व अवसर हमें प्रदान किया है। इसी से समस्त मानव-जाति का, माता जी की सभी सन्तानों का मुख्य कर्तव्य है कि जीवन की सभी प्रवृत्तियों में तथा उनके द्वारा माता जी की ही निरन्तर आराधना करने का सद्भाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इसे विस्मृत न करें।
हमें मानव-देह की जो भेंट प्राप्त हुई है, उसके लिए हमें आनन्द मनाना चाहिए। माता जी के यशोगान गाने तथा उनकी आराधना-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ करने की क्षमता का उपहार प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रफुल्लित होना चाहिए। आत्मसाक्षात्कार-रूपी चरम लक्ष्य के प्राप्त्यर्थ ही हमें यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। यदि हम इसका उपयोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति-रूपी माता जी के बाह्य स्वरूप की आराधना में करते हैं, तो कालान्तर में हम पर माता जी की कृपा होगी तथा वह सन्तों का सम्पर्क, उनकी कृपा, उनके उपदेश तथा उनकी ओर से मन्त्र-दीक्षा के रूप में इस आराधना का अन्तरंग स्वरूप प्रदान करेंगी। जैसे-जैसे हमारी आगे प्रगति होती जायेगी, वैसे-वैसे माता जी प्रथम मन्त्र-स्वरूप में प्रकट होंगी और तत्पश्चात् प्रकाश के मुख्यद्वार-रूप परम ध्यान-रूप में वह हमारे समक्ष प्रकट होंगी। अन्त में वह हमारी चेतना को समाधि द्वारा उद्भासित कर देंगी; क्योंकि व्यक्ति में माता जी का पूर्ण प्राकट्य समाधि तथा आत्मज्ञान के रूप में ही होता है। इस भाँति माता जी का साक्षात्कार होने पर जीवन का ध्येय प्राप्त हो जाता है, जीव कृतकृत्य हो जाता है और माता जी की आराधना पूर्ण हो जाती है। उसके कर्तव्य-कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह माता जी की अघटनघटनापटीयसी शक्ति-रूप में विलास कर रहे परब्रह्म के सच्चिदानन्द स्वरूप का शाश्वत आनन्द उपभोग करता है।
सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभंगरुचिभि-
वंशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः ।
स कर्ता काव्यानां भवति महतां भंगिरुचिभि-
र्वचोभिर्वाग्देवीवदनकमलामोदमधुरैः ।।'
(सौन्दर्यलहरी : १७)
चन्द्र-स्फटिक दरार सम सुन्दर, आद्या वासिन, मान।
ऐसे गुण से युक्त सरस्वति माता का जो करता ध्यान ।।
वह करता रचना काव्यों की, महती साहित्यिक उपमान ।
मधुर शब्द, मोहक भावों की, निर्गत मातु कंज-मुख मान ।।
हे माता, जो कोई भी वशिनी आदि वक्तृत्व-शक्ति प्रदान करने वाली देवियों के साथ, जो चन्द्रकान्त मणि के समान भास्वर हैं, तुम्हारा ध्यान करता है, वह महान् कवि बन जाता है। उसके शब्द मनोहर तथा मधुर होते हैं मानो सरस्वती के वदन-कमल की मधु हों।
नवम रात्रि
ॐ भूर्भुवस्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्'
अन्तिम मोक्ष का पथ
गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते ।
चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते ॥
ॐ त्रिलोकी-रूप सूर्य की ज्योति का करता हूँ ध्यान ।
जो जड़ चेतन अखिल विश्व की 'धी' करता प्रेरित छविमान ।।
गीता गंगा गायत्री गोविन्द बसें यदि अन्तर में।
हो चतुर्ग से युक्त नहीं फिर पुनर्जन्म कालान्तर में ।
जिनकी कृपा मात्र से प्रकृत साधकों की चेतना में परम तत्त्व का ज्ञान उद्भासित होता है, उन देवी को नमस्कार। जो सृष्टि, स्थिति व लय रूप रहस्यमय नाटक की सूत्रधार हैं, उन महिमामयी माँ को नमस्कार। जो अव्यक्त मनसातीत ब्रह्म को अपनी रहस्यमयी शक्ति से अनन्त नामरूपात्मक जगत् के मध्य में प्रकाशित करती हैं तथा जीव को माया से भ्रमित कर इस संसार-चक्र में आबद्ध करती हैं, उन्हें प्रणाम। जो अपने महासरस्वती-रूप में साधक को प्रपंच के मोहमय अस्तित्व से मुक्त कर सर्वोपरि आनन्द अथवा कैवल्यावस्था को प्राप्त कराती हैं, उन माता जी की विद्या माया को बारम्बार प्रणाम!
माता जी की नवरात्र की आराधना का आज नवाँ तथा अन्तिम दिवस है। आज उनकी ही परम करुणा तथा कृपा से उनकी पूजा करने तथा उनके चरण-कमलों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का हमें अमूल्य सुयोग प्राप्त हुआ है, जिससे हमारे मन तथा बुद्धि उन्नीत होंगे और हम जीवन के अन्तिम ध्येय आत्म-साक्षात्कार की ओर एक डग आगे बढ़ सकेंगे।
माता जी की कृपा असीम है। समस्त मानव जाति के प्रति तथा विशेषकर साधकों तथा जिज्ञासुओं के प्रति उनकी करुणा तथा उनका स्नेह अवर्णनीय है। माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए सदा आतुर रहती है। इसी भाँति यह जगज्जननी जिन्होंने इस क्षणस्थायी विश्व-नाटक की रचना की है तथा जो हमारे हृदय-कमल में विराजती हैं, वह अपने असीम वक्ष में अपने शिशुओं को वापस लेने को उत्सुक रहती हैं। जो बालक इस जागतिक खेल से श्रान्त हो चुके हैं तथा जिनकी खेल में रुचि नहीं रह गयी है, वे जब उनकी ओर मुख कर खड़े हो जाते हैं तथा 'माँ, माँ' कह उन्हें पुकारते हैं और कहते हैं, 'माँ, मुझे अब और अधिक खेलना नहीं है। मैं बहुत समय से तुमसे दूर पड़ गया हूँ। अब दया करो और इस बालक को अपने परम सुखमय क्रोड़ में पुनः उठा लो।' यही जीव का क्रन्दन है। यही मुमुक्षुत्व है। यही आकांक्षा है। यही असीम का ससीम के प्रति आह्वान है। जब ससीम जीवात्मा यह आह्वान सुनता है, तब वह इस नाटक से विरत हो कर उसकी ओर से मुख फेर लेता है और माता जी के मुखारविन्द की ओर दृष्टि-निक्षेप करता है। उस समय परमा माँ के करुणामय नेत्र कुछ काल के लिए उन्मीलित होते हैं और उनकी दिव्य दया की रश्मियाँ इस सन्तान पर पड़ती हैं और उसे प्लावित कर उसको इस विश्व-नाटक की क्लान्ति, अवसाद तथा धूलि से सदा के लिए मुक्त कर देती हैं और उसे आध्यात्मिक आनन्द की गूढ़ ऊँचाइयों पर पहुँचा देती हैं। वह माता जी के क्रोड़ में पुनः पहुँचता है तथा उसके विश्व-नाटक की चेष्टाएँ, सम्पूर्ण दुःख तथा कष्ट शेष हो जाते हैं। उसे निर्मल आनन्द, बहु-आकांक्षित स्वगेह में पुनः पहुँचने का आनन्द प्राप्त होता है।
हम सब पथिक हैं, अपने सच्चिदानन्द-रूपी परम धाम के, अपने मूल-स्थान के पथ-भ्रष्ट बालक हैं। हम चिर काल तक भटक चुके हैं और भटक कर अपने मूल-स्थान से बहुत दूर जा पड़े हैं-इसका ज्ञान होना तथा उस सच्चिदानन्द धाम की पुनर्प्राप्ति की तीव्र उत्कण्ठा जाग्रत करना ही आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है, उसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया है। यही आध्यात्मिक जीवन है और यही साधना-मार्ग है।
हम जान चुके हैं कि विद्या माया तथा अविद्या माया-ये दोनों ही परमा माता जी के स्वरूप हैं। इन उभय भावों द्वारा वह इस विश्व-नाटक के रंग-मंच पर दुर्गा, लक्ष्मी तथा सरस्वती-इन तीनों रूपों में लीला करती हैं। कल हमने देखा कि माता सरस्वती ओंकाररूपिणी, नादरूपिणी स्वरूप में अपने परम सात्विक रूप में तथा मनुष्य की बाह्य प्रवृत्तियों में प्रवृत्ति-रूप में किस प्रकार व्यक्त होती हैं। माता जी परम विद्या स्वरूप होते हुए भी उनमें अविद्या का भी किंचिद् गूढ़ अंश रहता है और इस अविद्या माया के स्वरूप में वह प्रवृत्ति में सरस्वती-तत्त्व के रूप में प्रकट होती हैं।
परन्तु सरस्वती माता मुख्यतः विद्यारूपिणी हैं तथा भव्य विद्या माया स्वरूप में ही वह जीव के आन्तरिक जीवन में, निवृत्ति-पथ में अनेकविध रूपों में अपने को अभिव्यक्त करती हैं। आन्तरिक जीवन में, निवृत्तिपरक जीवन में प्रकट होने वाले माता जी के इस स्वरूप का ध्यान अपने समक्ष रख कर हम आज उनके चरण-कमलों में अपनी श्रद्धा तथा भक्ति अर्पित करेंगे। हम देख चुके हैं कि वह प्रवृत्ति के लिए सर्जनात्मक शक्ति हैं और हमने यह भी देखा कि वह रचनात्मक शक्ति क्योंकर हैं? सभी वस्तुओं के आरम्भ में वह ही निवास करती हैं। वैज्ञानिकों की गवेषणा-शक्ति माता जी हैं। कविता के उपासक कवियों की कवित्व-शक्ति माता जी ही हैं। वही संगीतकार, चित्रकार, शिल्पकार तथा अन्य ललित कलाओं के कलाकारों की कला-विषयक प्रतिभा है। गहन अन्वेषण-काल में किये हुए वैज्ञानिकों के आविष्कार भी माता जी हैं। बाह्य प्रकृति के तीव्र बौद्धिक चिन्तन से जो भी नव-सर्जन होता है, वह भी माता जी का स्वरूप ही है। इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विविध पदार्थों में माता जी ही हैं। सभी रचनात्मक कार्य-रूप में माता जी ही विलास करती हैं। सभी व्यवसाय तथा सभी व्यापार माता जी के ही स्वरूप हैं। श्रेष्ठ विक्रेताओं की व्यावसायिक कुशलता भी माता जी हैं। मानव-जगत् के बाह्य क्षेत्र में, प्रवृत्ति में वह शिक्षा-रूप में व्यक्त होती हैं। इस भाँति माता जी बाह्य जगत् में नानाविध रूपों में प्रकट होती हैं।
अनेक में से एक अद्वितीय सर्वोत्कृष्ट उद्गम स्थान की ओर पीछे मुड़ने की माता जी की विशिष्ट प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया के विषय में हमने विचार किया। निवृत्ति-मार्ग में साधक आत्मा के अन्तर्मुखी जीवन में, जीव के योग तथा साधना-पथ के आन्तरिक जीवन में माता जी गुरु-दीक्षा रूप में किस प्रकार प्रकट होती हैं, इसे भी हम देख चुके हैं। मन्त्र, मन्त्र जप तथा अनुष्ठान जैसी मन्त्र-साधना आदि भी माता जी हैं। स्वच्छ शुभ्र वसन तथा दिव्य सौन्दर्य से वह विशुद्ध सत्त्वशीलता की साकार रूप हैं, यह भी हम देख चुके हैं।
माता जी : परम सत्त्वस्वरूप
आध्यात्मिक साधक के हृदय में माता जी सत्त्व-रूप में प्रकट होती हैं तथा साधक पर जब सरस्वती माता जी की कृपा उदय होती है, तो उसका समस्त जीवन रूपान्तरित हो जाता है। उसके सभी प्रकार के आसुरी तथा पाशविक भाव शनैः शनैः पर निश्चित रूप से विलय को प्राप्त होते हैं; क्योंकि सत्त्व के शुभ्र उज्ज्वल वर्ण के आलोक के समक्ष तमस् का अन्धकार ठहर नहीं सकता। मानव-जीवन में सत्त्व एक श्रेष्ठ सकारात्मक गुण है। अतः माता सरस्वती के कृपा-स्वरूप सत्त्व के आविर्भाव से तमोगुण क्षीण होने लगता है तथा अन्त में साधक तमोगुण के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। इन्द्रियों की अत्यन्त निम्न प्रकार की क्षुधा, जो उसे एक समय अतीव सुखदायक प्रतीत होती थी तथा जिसमें वह पहले रचा-पचा रहता था, अब उसे दुःखरूप लगने लगती है। वह उससे घृणा करता है। जिसके जीवन में माँ सरस्वती विराजती हैं, उसके जीवन से स्थूल मलिन भाव अदृश्य हो जाते हैं।
व्यक्ति में वर्तमान रजोगुण में भी परिवर्तन आता है। स्वार्थमयी वृत्तियों से जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वे सब रजोगुणी प्रवृत्तियाँ कही जाती हैं। लोभ, तृष्णा तथा स्वार्थमयी वृत्ति से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियाँ राजसिक होती हैं। कार्यशीलता अथवा गतिशीलता सदा ही अच्छी है। किसी भी ध्येय के प्राप्त्यर्थ किये जाने वाले प्रत्येक प्रयास और प्रयत्न में वह अमूल्य परिसम्पत्ति है, किन्तु यह गतिशीलता जब स्वार्थ, लोभ तथा तृष्णाजनित तथा मानव-सत्ता के इन अकुलीन तत्त्वों से निर्देशित होती है, तब रजोगुण मनुष्य को बहिर्मुखी बना कर उसे अधिकाधिक दृढ़ बन्धन में आबद्ध कर लेती है। किन्तु जब साधक के जीवन में महत्तर शक्ति का उच्चतर दिशा की ओर खिंचाव बढ़ता है और सत्त्व-शक्ति उसके निवृत्ति-मार्ग में प्रकट हो कर कार्य करना आरम्भ कर देती है, तब साधक में अन्तर्निहित रजोगुण के ऊपर उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ने लगता है।
रजस्-जो अब तक स्वार्थपरता तथा लोभ का सहायक था, वही रजस्- वशीभूत होने तथा व्यपवर्तित हो उच्चतर तथा श्रेष्ठतर मार्ग द्वारा प्रवाहित होने लगता है। उसमें वर्तमान रजोगुणी गति-शक्ति तमस् के बदले सत्त्व से सम्बद्ध हो जाती है, जिसके परिणाम-स्वरूप यह शक्ति उसके आध्यात्मिक जीवन में एक अमूल्य परिसम्पत्ति बन जाती है। अब इसे नियन्त्रित तथा परिष्कृत कर उच्च तथा अभिजात आध्यात्मिक कार्यों की दिशा में व्यपवर्तित कर दिया जाता है। अब उसकी गतिशीलता परोपकारी कार्यों में परिणत होती है और वह करुणा, दया, निःस्वार्थता जैसे शुद्ध सात्त्विक गुणों से अनुप्राणित होता है। वह सभी प्राणियों में विद्यमान तथा उनके रूप में प्रकट भगवान् की कर्मयोग अथवा सेवा के रूप में आराधना करने की शुद्ध भावना से प्रेरित होता है। इस भाँति आध्यात्मिक पथ में आने वाले तमस् तथा रजसू जैसी निम्न प्रकृति के व्यवधान दूर हो जाते हैं। तमोगुण समाप्त हो जाता है। दैनिक निद्रा आदि के रूप में अंशतः प्रकट तमोगुण के अतिरिक्त उसके अन्य स्थूल रूपों का नाश होता है। जब माँ सरस्वती कृपा कर साधक के निवृत्ति-परायण जीवन में शुद्ध सत्त्वगुण के रूप में प्रकट होती हैं, तब रजोगुण भी उसका (साधक का) मित्र तथा सहायक बनने लगता है।
श्रीमद्भगवद्गीता के सतरहवें अध्याय में समस्त गुणों तथा पदार्थों को सत्त्व, रज तथा तम-इन तीन विभागों में वर्गीकृत किया गया है। यदि आप इस गुणत्रय- विभाग को पढ़ें, तो आपको ऐसा लगेगा कि जिन पदार्थों का वर्णन 'सात्विक तत्त्व' के रूप में किया गया है, वे सब माता सरस्वती के ही स्वरूप है। साधक तथा मुमुक्षु के जीवन में माता जी स्वयं योग तथा साधना के रूप में प्रकट हैं और अन्त में वह उसकी चेतना का ज्ञान-विभा रूप में उद्घाटन का स्वरूप धारण करती हैं। साधक की प्रवृत्ति में सत्व-रूप में माता जी सदाचार के रूप में व्यक्त होती हैं। हमें ज्ञात है कि सदाचार ही आध्यात्मिक जीवन में समस्त सफलताओं का आधार है। यह नींव का कार्य करता है। राजयोग के यम-नियम सदाचार के अतीव विज्ञानसम्मत रूप हैं।
गुरु के वचन वेदवाक्य हैं
दीक्षा-समय में गुरु से प्राप्त गुरु-मन्त्र ही परम शब्द है। माँ इस वाक् या शब्द के मध्य से ही परम तत्त्व के रूप में प्रकट होती हैं। यदि माता के मन्त्रात्मक स्वरूप की सम्मानपूर्वक आराधना करनी हो, तो सद्गुरु से प्राप्त मन्त्र का सतत निष्ठापूर्वक जप करना चाहिए। यदि हम इस मन्त्र की अवज्ञा करें, गुरु-प्रदत्त नाम की अवहेलना करें और उसके जप में उत्साह न प्रकट करें तो यह माँ की पूजा में त्रुटि मानी जायेगी, माँ सरस्वती की पूजा की अवज्ञा कही जायेगी। हम यदि इस प्रकार माँ का अनादर करेंगे, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी।
सामान्य रीति से, साधक के योग-मार्ग तथा आध्यात्मिक जीवन में गुरु की शिक्षाओं तथा उनके दिन-प्रति-दिन के उपदेशों के रूप में स्वयं माता जी प्रकट होती हैं। अतएव साधक की अभिवृत्ति भक्तिभावपूर्ण होनी चाहिए तथा गुरु के उपदेशों को अतीव श्रद्धा तथा गम्भीर भाव से श्रवण तथा अनुशीलन करना चाहिए। उसमें असावधान नहीं होना चाहिए। उसे गुरु के वचन को सामान्य वाणी मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। साधक के लिए गुरु-वचन ही वेदवाक्य हैं; क्योंकि वे उसके लिए मन्त्र के समान हैं- 'मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्।'
इन दिनों गुरु के सामान्य वचनों को सामान्य शब्द मान कर उन पर यथोचित मनोयोग न देने की भूल साधक-जगत् में बहुत अधिक प्रचलित हो चली है। सद्गुरु के सान्निध्य में रहने वाले साधकों तथा शिष्यों में उनके उपदेश तथा वाणी द्वारा प्रकट होने वाली सरस्वती का आदर कर उन्हें ग्रहण करने में सामान्यतः शिथिलता आ जाती है, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक क्षति उठानी पड़ती है। इसलिए गुरु-वाणी-रूप में व्यक्त होने वाली माता जी के इस स्वरूप के प्रति अपनी अभिवृत्ति में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि हम उन्हें यथोचित भाव से ग्रहण करें और निष्ठापूर्वक उनका पालन करें, तभी हम माता सरस्वती की कृपा का उचित तथा लाभप्रद उपयोग करेंगे।
स्वाध्याय तथा उसका व्यावहारिक मूल्य
आध्यात्मिक साधना में इसके अतिरिक्त माता जी अन्य दो विशिष्ट रूपों में प्रकट होती हैं। हम कह चुके हैं कि सरस्वती माता वेदों की प्रतिमूर्ति हैं। वेद का अर्थ है परमात्मा का अलौकिक ज्ञान। उपनिषद् वेदों का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। उपनिषदों का सारतत्त्व मानव-जाति तक भगवद्गीता द्वारा पहुँचाया गया है। अतएव, माता जी साधक के समक्ष इस अपूर्व सार्वभौमिक ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता के रूप में प्रकट हुई हैं। इसी कारण सभी आध्यात्मिक आचार्यों ने गीता के नित्य नियमित पाठ का निर्देश दिया है। यदि हम प्रतिदिन गीता का स्वाध्याय करें तथा उसमें दिये हुए सिद्धान्तों को शनैः-शनैः अपने जीवन में आत्मसात् करने का प्रयत्न करें, तभी गीता-रूप में प्रकट हुई माता सरस्वती की आराधना होगी। जो साधक पूज्य गुरुदेव के चरण-कमल में रह कर दिव्य जीवन यापन में प्रयत्नशील हैं, उन सभी के लिए निर्धारित 'दिनचर्या' में गीता के स्वाध्याय पर विशेष बल दिया गया है। हम यह भी जानते हैं कि पातंजल योग-दर्शन के 'नियम' का स्वाध्याय एक महत्त्वपूर्ण अंग है।
परा शब्द अथवा मूल शब्द स्वरूपा माँ सरस्वती विकास के क्रम से प्रथम ध्वनि, तत्पश्चात् वाणी अथवा वाक् तथा तदनन्तर वर्णमाला के अक्षर-रूप में प्रकट होती हैं। उसके पश्चात् अक्षरों के संयोजन से नाम बनते हैं तथा नाम का अर्थ और उसके साथ रूप प्रकट होता है। यह सब हम पहले देख चुके हैं। इस भाँति अपने धर्मशास्त्रों में माता जी अक्षर-रूप में प्रकट हुई हैं। इससे अपने सभी धर्मशास्त्र तथा आध्यात्मिक ग्रन्थ सरस्वती-तत्त्व के पुंजीभूत रूप हैं। लिखित अक्षरों तथा शब्दों के रूप में माता जी ही परब्रह्म का ज्ञान हमें प्रदान करती हैं। अतः जब हम नित्य स्वाध्याय में आध्यात्मिक ग्रन्थों का पाठ करते हैं, तब हम वस्तुतः शब्द-रूप में उसमें निवास कर रही माता सरस्वती के सम्पर्क में आते हैं और वह हमारा प्रत्यक्ष मार्ग-दर्शन करती हैं।
स्वाध्याय दैनिक साधना का एक प्रधान अंग है। साधक के जीवन में इसका महत्त्व अनेकविध है। स्वाध्याय साधना के क्षेत्र में जो महत्त्वपूर्ण भाग अदा करता है, उसके कम-से-कम एक अंग पर हम अभी विचार करेंगे; क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह साधक के विचार तथा भाव में सत्त्व तथा दैवी गुणों के संवर्धन में क्योंकर सहायक होता है? मनुष्य की आध्यात्मिक साधना का प्रकार तथा उसका सम्पूर्ण स्वरूप उसके संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। मन सब-कुछ है और मन संस्कारों का गट्ठर मात्र है। इन संस्कारों का सृजन व्यवहार से होता है। बाह्य पदार्थों के सम्पर्क तथा मनुष्यों के संसर्ग से अपने मन के ऊपर संस्कारों की अधिकाधिक छाप पड़ती है। बाह्य व्यवहार जगत् में और उसमें भी विशेषकर कर्मयोग के क्षेत्र में नितान्त अनात्मिक स्वरूप के संस्कार प्राप्त होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन तथा आध्यात्मिक विकास के पूर्णतया विरोधी होते हैं।
मनुष्य के दैनन्दिन जीवन की सामान्य बाह्य प्रवृत्तियों में से नित्यप्रति व्यवहार के, प्रवृत्तियों के तथा विषयों के संस्कार प्रचुर मात्रा में पैदा होते हैं। यदि ऐसे संस्कार दिन-प्रति-दिन बढ़ते गये, तो वे व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाते हैं। वे उसको बहिर्मुखी बनाते हैं तथा उसके मन को अधिकाधिक विषयाकार बनाने वाली भयानक शक्ति बन जाते हैं। परन्तु ऐसे संस्कारों से सर्वथा दूर रहना भी शक्य नहीं है। अधिकांश आध्यात्मिक साधकों के लिए ऐसे समस्त व्यवहारों का पूर्ण रूप से त्याग करना सम्भव नहीं है। इसीलिए उन्नतकारी धर्मग्रन्थों के नित्य स्वाध्याय द्वारा पवित्र आध्यात्मिक विचारों को मन में प्रविष्ट कर इस प्रकार के संस्कारों का, इस प्रकार के विचारों का प्रतिकार करने के लिए सुन्दर मनोवैज्ञानिक शोध की गयी है।
नित्य, नियमित रूप से आयासपूर्वक किये गये स्वाध्याय से साधक प्रतिदिन जीवन के उन्नायक तथा रूपान्तरकारी विशुद्ध आध्यात्मिक विचार-पुंज ग्रहण करता है जिससे उसके मन में प्रबल सकारात्मक, सात्त्विक तथा आध्यात्मिक संस्कारों की छाप पड़ती है जो दैनिक जीवन-व्यवहार में अपरिहार्य रूप से एकत्रित हुए अशुभकारी लौकिक संस्कारों को पराभूत करने में सहायक होते हैं। साधक में नवीन भाव जाग्रत करने की उनमें क्षमता होती है। वे साधक के विचारों, संस्कारों तथा स्वयं भावों को रूपान्तरित कर देते हैं। सन्तों की जीवन-गाथाओं, गीता, भागवत, रामायण, बाइबिल, कुरान, जेन्द अवेस्ता, धम्मपद आदि के दैनिक स्वाध्याय द्वारा माता सरस्वती के साथ सम्बन्ध-स्थापन से साधक के स्वभाव को सात्त्विक तथा आध्यात्मिक विचारों का आहार नियमित रूप से मिलता रहता है।
हमें ऐसा लगता है कि मन में इस प्रकार के शक्तिशाली, निश्चयात्मक तथा आध्यात्मिक विचार-समूह का सृजन धारणा तथा ध्यान-काल में बहुत सहायक होता है। साधक जब ध्यान करने का प्रयास करता है, तभी उसका मन बाहर भटकने लगता है। ध्यान की प्रारम्भिक अवस्था में मन के भटकने की वृत्ति बहुत बलवती होती है। यह समस्त प्रक्रिया नीचोपरि की क्रीड़ा-सी, एक प्रकार का विरुद्धाकर्षण-सी होती है। मन भटकने लगता है और साधक उसे पुनः पुनः लक्ष्य पर केन्द्रित करता है। यहाँ एक अवांछित परिस्थिति उपस्थित होती है कि मन स्थूल, वैषयिक तथा लौकिक विचार-क्षेत्र में ही रमण करता है।
सतत अभ्यास तथा तीव्र वैराग्य के बिना मन की भ्रमणशीलता को रोकना सम्भव नहीं है; परन्तु किंचित् परिवर्तन अवश्य शक्य है। यदि नित्य नियमित स्वाध्याय द्वारा मन में सात्त्विक तथा शक्तिशाली विचारों का सिंचन किया जाये, तो ध्यान में विक्षेप के समय उनका भ्रमण क्षेत्र धीरे-धीरे सात्त्विक बन जाता है। मन विषयी विचारों में भटकने के स्थान में अब पवित्र विचारों, उदात्त विचारों तथा सात्त्विक विचारों में विहार करता है। मन का यह भ्रमण साधक के लिए अधिक हानिकारक नहीं होता। इस भाँति भी 'स्वाध्याय' साधक के जीवन में एक अमूल्य परिसम्पत्ति है।
मितभाषी बनो
आइए, अब हम साधक के आचार के सम्बन्ध में विचार करें। हम अब साधकों के नित्य आचार में अतीव उपयोगी कतिपय सूचनाएँ देंगे। हम देख चुके हैं कि वाणी माता सरस्वती का स्वरूप है। माँ सभी प्राणियों में 'वाकू' रूप में प्रकट होती हैं। माता जी वाक्शक्ति हैं। नियमपूर्वक मौन द्वारा वाणी का संयम करना भी माता सरस्वती की आराधना ही है। इस प्रकार माता जी की वाक्शक्ति संचय करने से शक्ति-संग्रह होता है जिसका उपयोग प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान जैसी योग की प्रक्रिया में किया जाता है। मौन-साधना द्वारा संचित वाक्शक्ति, विवेक, विचार तथा आत्म-विश्लेषण के प्रयास में बहुत सहायक होती है। यह तो व्यवहार में अनुभूत ज्ञान है। कोई भी साधक मौनाभ्यास द्वारा इसका स्वयं अनुभव कर सकता है। जब तक वाणी का, वाक्शक्ति का व्यय होता है, मन बहिर्मुखी होता है, तब तक सूक्ष्म विचार तथा आत्म-निरीक्षण शक्य नहीं है; परन्तु जब मौन द्वारा वाक्शक्ति का संचय किया जाता है, तभी मन अन्तर्मुखी बनता है तथा उसके परिणाम स्वरूप विवेक, विचार तथा आत्म-निरीक्षण करना सम्भव हो पाता है।
सत्य बोलो
वाक्शक्ति की पवित्रता बनाये रखने का महान् उत्तरदायित्व साधक के शिर पर है। वाणी-स्वरूप में रहने वाली माता सरस्वती की शक्ति की पवित्रता की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम जानते हैं कि असत्य अनिष्टकारी तथा आत्म-विरोधी है। अतएव, परम सत्य अथवा आत्यन्तिक सत्य के साक्षात्कार के आकांक्षी साधक को अपनी वाणी में उस सत्य को प्रकट करने का सदा सावधानीपूर्वक प्रयास करना चाहिए। सत्य बोलने का नियम लेने से वाणी में जो विमलता आती है, वह अतीव महत्त्व की है। सत्यवादिता के महान् सद्गुण का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यदि साधक में सत्यवादिता नहीं है, तो उसका सम्पूर्ण आध्यात्मिक जीवन ही निष्फल हो जाता है। उसका जीवन शून्यवत् है।
सत्य में पूर्णतया टिके रहने की अपनी सम्पूर्ण शक्ति तथा पूर्ण हृदय से प्रयास किये बिना साधक के जीवन में रंच मात्र भी सच्ची, ठोस तथा स्थायी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। इस विषय में कोई मध्यवर्ती मार्ग नहीं है। मनुष्य या तो सत्यवादी होता है अथवा असत्यवादी। जब तक साधक पूर्ण रूप से सत्यवादी नहीं बनता, तब तक आध्यात्मिक प्रगति उसके लिए दुराशा अथवा स्वप्न मात्र है। वह कभी भी साकार नहीं हो सकती। यह एक अटल सत्य है। अतः यदि साधक अपनी साधना के प्रति गम्भीर है, अपनी खोज में निष्ठावान् है, यदि उसमें इस मर्त्यशील भौतिक जीवन के कष्ट और शोक से, रोग तथा मृत्यु से संकुल इस पार्थिव जीवन के पाश को विदीर्ण करने की सच्ची ज्वलन्त कामना है, यदि अपने को मुक्त कर शाश्वत आनन्द भोगने की उत्कण्ठा है तो उसे सत्य का अटल उपासक बनना ही पड़ेगा; तभी माता करुणावश हो उसके ऊपर कृपा करेंगी तथा उसे परम सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा।
माता सरस्वती के परम वैभवशाली तथा परम तेजोमय स्वरूप तथा सद्गुणों के शिरोमणि तुल्य 'सत्य' पर नित्यप्रति निश्चित रूप से ध्यान करने का हम आज से हो संकल्प लें। सत्य के स्वरूप में माता जी की आराधना करने से हृदय में आत्मा की ज्योति प्रतिष्ठित होगी। जब तक व्यक्ति के हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक उसमें आत्म-ज्योति प्रकाशित नहीं हो सकती। अतः हमें माता सरस्वती का सत्य-रूप में नित्यप्रति ध्यान करना चाहिए।
सत्य ही महान् योग है। इस कलियुग में सत्य ही महानतम तप है। जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। माता सरस्वती के सत्य-स्वरूप की परम महिमा का हमें अपने मन में ध्यान रखना चाहिए। उस पर ध्यान करना चाहिए। उसका चिन्तन करना चाहिए। हमारे विचार, हमारी वाणी तथा हमारे कर्म में सत्य अनून रूप से प्रकाशित हो, इसके लिए हमें प्रत्येक सम्भव उपाय द्वारा निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए। इस अत्यावश्यक किन्तु अतीव दुष्कर कार्य में माता जी की कृपा हमारी सहायता करे!
प्रिय बोलो
भाषा, वाणी एक सर्वशक्तिशाली वस्तु है, इस मानव-लोक में एक महान् शक्ति है। वाणी का उपयोग रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों के लिए भी किया जा सकता है तथा संहारक और विनाशकारी कार्यों के लिए भी हो सकता है। समस्त सर्जन का मूल माता सरस्वती ही हैं, यह हम पहले देख चुके हैं। अतः प्रत्येक साधक को इस महान् वाक्शक्ति के उपयोग में सदा सावधान रहना चाहिए। परमात्मा द्वारा सृजित क्षुद्रतम प्राणी के मन को भूल कर भी कठोर शब्दों के प्रयोग द्वारा न दुखाने का उसे संकल्प लेना चाहिए।
जिस वाणी से किसी को आघात पहुँचे, ऐसी कठोर वाणी का साधक को सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसे मधुर वाणी बोलनी चाहिए। यदि किसी समय मधुर वाणी बोलना शक्य न हो, तो ऐसे समय में मौन-सेवन ही श्रेयस्कर है। इससे निम्नतर कोटि की बात यह होगी कि जिसके प्रति कठोर शब्दों को व्यवहृत किया हो, उससे तुरन्त खेद प्रकट करते हुए क्षमा-याचना की जाये। पर यह तो निकृष्ट कोटि के लोगों की बात है। हमें तो सदा उत्तम अधिकारी बनने का आकांक्षी होना चाहिए अर्थात् हमारी वाणी सदा ही नितान्त मधुर होनी चाहिए। इन तीन बातों को ध्यान में रखें-मित भाषण, सत्य भाषण तथा मधुर भाषण।
अपनी वाणी पर संयम रखें
मैं एक बार पुनः कहूँगा कि विश्व की सर्जन-शक्ति माँ सरस्वती-स्वरूपा वाणी का उपयोग दूसरों के सहायतार्थ करना चाहिए। हमारी वाणी निरर्थक न हो। बोलने की आवश्यकता पड़े, तो भगवान् के विषय में तथा विश्व के अन्य उन्नत आदर्शों के विषय में ही चर्चा करें। दूसरों को आश्वासन देने, प्रेरणा देने, मार्ग-दर्शन करने, शिक्षा देने अथवा अन्य किसी रूप में सहायक होने में ही माता सरस्वती की वाणी-शक्ति का उपयोग करें। आध्यात्मिक साधना तथा सत्य की आध्यात्मिक खोज के क्षेत्र में निरर्थक बातचीत का सर्वथा परिहार करना चाहिए। व्यर्थ के वार्तालाप से शब्द-शक्ति अथवा वाक्शक्ति में निवास करने वाली माता सरस्वती का अपमान होता है।
साधक को कभी भी अश्लील शब्द नहीं बोलने चाहिए। एक बार आदत पड़ जाये, तो उसको छोड़ना कठिन हो जाता है और उसमें भी बुरी आदतों के विषय में तो यह कथन अक्षरशः सत्य है। बुरी आदतों की अपेक्षा अच्छी आदतों का त्याग करना सरल है; क्योंकि बुरी आदतें मनुष्य की निम्न प्रकृति में दृढ़ता से खचित होती हैं। इस प्रकार के आचरण की भूतकाल में बारम्बार पुनरावृत्ति होने से ये बुरी आदतें उसके स्थूल पाशवी अंग में दृढ़ता से मूलबद्ध हो जाती हैं। आज संसार में पचहत्तर प्रतिशत अशिष्ट और पचीस प्रतिशत शिष्ट वाणी का व्यवहार में उपयोग देखने में आता है। अधिकांश लोगों के लिए तो अश्लील तथा अशिष्ट शब्दों का दैनिक बातचीत में उपयोग एक सामान्य बात हो गयी है। उन्हें उनमें कुछ विशेष अनौचित्य नहीं प्रतीत होता है; किन्तु साधक के जीवन का यही मानदण्ड नहीं होना चाहिए। साधक को अपनी वाणी में आपत्तिजनक शब्दों तथा पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी वाणी गंगा जी के पवित्र जल की भाँति निर्मल होनी चाहिए।
विशुद्ध सत्त्व-रूप में माता सरस्वती को व्यक्त करने के ये सब मार्ग हैं। ये सब आध्यात्मिक सद्गुण हैं और अपने में सत्त्व की वृद्धि करने में सहायक होते हैं तथा उसके आध्यात्मिक विकास में सीधे योगदान देते हैं।
साधक के आभ्यन्तरिक मार्ग में निवृत्ति-स्वरूप में प्रकट होने वाली भगवती माँ के विविध रूपों को हमें स्मरण रखना चाहिए। आज आपके सम्मुख ये थोड़े से रूप प्रस्तुत किये गये हैं। इस विषय में यदि हम विचार करें, तो हमें पता चलेगा कि माता जी किन विविध रूपों से साधक के व्यक्तित्व को आपूरित करने का प्रयत्न करती हैं। जब हम सत्त्वगुण के विरोधी तत्त्वों से अवगत हो जायेंगे, तब माता सरस्वती के स्वरूप के विरोधी सभी कार्यों का परिहार कर सकेंगे तथा अपने आन्तरिक जीवन तथा स्वभाव के उन तत्त्वों को उत्पन्न करने, विकसित करने तथा वृद्धि करने के लिए श्रम करेंगे जिनमें वे विशेष रूप से प्रकट हैं। हम अशुद्ध तथा अध्यात्म-विरोधी वस्तुओं का परित्याग कर देंगे और अपने स्वभाव को अधिक-से-अधिक शुद्ध, सात्त्विक बनायेंगे। अन्त में हम अपने को आध्यात्मिक चेतनावस्था में पूर्ण रूप से विकसित करने में सफल होंगे जिसके परिणामजन्य अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर स्वरूप-ज्ञान प्राप्त करेंगे और तब यह घोषित कर सकेंगे- "मैं न तो मन हूँ और न यह शरीर ही। मैं अमर आत्मा हूँ।"
"शुद्धोऽहं, बुद्धोऽहं, निरंजनोऽहं, संसारमायापरिवर्जितोऽहम्,”
“देहो नाहं जीवो नाहं प्रत्यगभिन्नो ब्रह्मैवाहम्, "
"सच्चिदानन्द स्वरूपोऽहम्।"
ना मैं मन हूँ, ना मैं तन हूँ, अमर आत्मा का हूँ रूप।
शुद्ध भी हूँ, बुद्ध भी हूँ मैं, और निरंजन का हूँ रूप ॥
जग की माया पार कर चुका, देव नहीं ना जीव का रूप।
सबसे भिन्न ब्रह्म ही हूँ मैं 'सत्-चित्-आनन्द' शुद्ध स्वरूप ।।
जिस साधक ने माता सरस्वती की सच्चे हृदय से आराधना की है तथा जिसने माता सरस्वती की कृपा प्राप्त कर ली है और माता सरस्वती जिसका प्रथम प्रकट रूप हैं, उस परमात्मा का प्रकाश जिसे प्राप्त हुआ है, उस साधक के ये सहज उद्गार हैं।
इडा देवहूर्मनुर्यज्ञनीबृहस्पतिरुक्थामदा निश सिषद्विश्वे देवाः सूक्तवाचः पृथिवि मातर्मा मा हि सीर्मधु मनिष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यास शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ।'
इडा, देव, मनु, यज्ञ की देवी, बृहस्पति कहते मधुर।
विश्वदेव सुन्दर सूक्ति से युक्त वाक्य कहते मधुरं ।।
पृथ्वी माता देव आदि करते प्रेरित विचार मधुर।
मधुर हूँ कहता, मधुर कहूँगा, देवोप्रिय वाणी मधुर ।।
अतः पालने योग्य मनुष्यों को सत्यं वाणी मधुरं।
रक्षा करते देव, समर्थन पितर करें, शोभा मधुरं ।।
विजयादशमी
महान् लक्ष्य तथा उसकी उपलब्धि
तवामृतस्यन्दिनि पादपंकजे
निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति ।
स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिर्भर
मधुव्रतो नेक्षुरसं हि वीक्षते ।।
चरण कमल से निःसृत अमृत में प्रविष्ट जिसकी आत्मा।
कैसे भजे अन्य थल को जब लगन लगी हो तुझमें माँ ।।
ज्यों पराग में लीन भ्रमर हो, कमल मध्य में स्थित माँ।
मधुर ईख-रस क्योंकर चाहे, चखकर भक्ति-अमिय रस माँ।
आज माता जी के विजय-दिवस का महोत्सव है। इस विजय दिवस पर समस्त देव प्रसन्न होते हैं तथा समस्त मानव जाति आनन्दातिरेक में मग्न होती है; क्योंकि उन्हें यह परमोत्कृष्ट आश्वासन प्राप्त हुआ है कि वे यदि विपद् और आपद् में पड़ कर सहायतार्थ माँ की ओर मुड़ेंगे, तो माँ उन्हें शक्ति और साहाय्य अवश्य प्रदान करेंगी; क्योंकि जो विपत्ति में पड़ कर माँ के दिव्य चरणों में शरणापन्न होता है, माँ उसकी रक्षा करती हैं। माता जी अनन्त शक्ति का आधार महाशक्ति हैं। अतः उनके सम्मुख जाते ही हमारी निर्बलता तिरोहित हो जाती है। समस्त अमंगल, अज्ञान तथा मोह की शक्ति के ऊपर महत् जय-लाभ का कार्य सम्पन्न होता है और माता जी के साथ विजयोत्सव का आनन्द मनाते हैं। विजयादशमी साधक के विश्वास, शक्ति तथा साहस-प्राप्ति का परम दिवस है।
इस दिवस को सभी साधकों तथा भगवान् की खोज में रत भक्तों को महाशक्ति तथा साहस प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि माँ ने उनके दिव्य भाव के पूर्णाधार रूप में प्रकाशित होने के मार्ग में अन्तराय-रूप में आने वाली आसुरी शक्ति को ध्वंस कर परब्रह्म के धाम के प्रवेश-द्वार को उद्घाटित कर दिया है। आज के परम पवित्र दिवस पर माता जी की आराधना महामाया के परम विशुद्ध विद्या-स्वरूप का पूजन है। आज तक नवरात्र के दिनों में मानव-व्यवहार के इस दृश्य जगत् में प्रकट हुए माता जी के विविध रूपों की उपासना हमने की, किन्तु विजयादशमी के दिन से माता जी के विद्या और अविद्या-रूपी बाह्य स्वरूपों के परे पराशक्ति के विशुद्ध विद्या माया के मुखारविन्द का हम दर्शन करते हैं। इस रूप का दर्शन करना स्वयं परब्रह्म की अगाध तथा अतल गहराइयों का दर्शन करना है।
कारण, हमने इस पूजा के प्रारम्भ में यह कहा था कि माँ परब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। वह परब्रह्म ही माता जी हैं। अतएव, अपने विशुद्ध विद्या माया रूप में वह स्वयं परब्रह्म है। इसी से आज इस परम महान् तथा मंगलकारी विजयादशमी के दिवस पर माँ के उस अत्युज्चल दीप्तमान विद्या-रूप को, आत्मज्ञान-प्रकाशक रूप को हम प्रणाम करते हैं।
आज के दिन निम्न-भाव का किसी भी रूप में अस्तित्व नहीं है। किसी प्रकार की आसुरी सम्पत्ति नहीं रह गयी है। क्षुद्र वृत्ति का कोई चिह्न अवशेष नहीं रहा है। अन्धकार पूर्ण रूप से ध्वस हो गया है। इसका पूर्ण तिरोभाव हो गया है। वहाँ एकमात्र माँ का साम्राज्य व्याप्त है। माँ इस समय असीम चिद्घन हैं। माँ के इस तेजोमय स्वरूप की उपासना उस परब्रह्म की श्रेष्ठ उपासना में अपने को विसर्जन करना है। इस भाँति अब हम उस परब्रह्म की पूजा तथा उपासना आरम्भ करते हैं जहाँ पहुँच कर जन्म-मृत्यु का दुष्ट चक्र समाप्त हो जाता है। यही वह शाश्वत प्रकाश का धाम है जहाँ जाने के पश्चात् शोक तथा दुःख में प्रत्यावर्तन नहीं होता। हम उस परम धाम को सदा के लिए प्राप्त कर लेते हैं जो कि समस्त शोकों, समस्त कष्टों तथा मोहों से परे है। यह साधक, जिज्ञासु तथा समस्त मानव का चरम लक्ष्य है। वास्तव में एकमात्र इस सर्वोच्च ध्येय की उपलब्धि के लिए ही हमें इस जगत् में यह मानव-जन्म प्राप्त हुआ है। संसार के अन्य पदार्थों के प्राप्त्यर्थ अपनी भाग-दौड़ भ्रामक एवं निरर्थक है। इस अमूल्य जन्म का एकमात्र आशय, उद्देश्य तथा लक्ष्य परब्रहा का साक्षात्कार करना है।
गुरु : परब्रह्म की स्थूल मूर्ति
आज के यशस्वी दिवस को आध्यात्मिक जीवन के अतीव गुप्त रहस्य पर विचार करने के अवसर का लाभ उठायें। इस दृश्य जगत् में विलस रही, साधक में भिन्न-भिन्न गुणों द्वारा व्यक्त हुई तथा मनुष्य के जीवन और उसकी प्रवृत्तियों में भिन्न-भिन्न स्वरूपों में प्रकट हुई माँ के दुर्गा, लक्ष्मी तथा सरस्वती-इन त्रिविध रूपों का हमने विचार किया; परन्तु इन सबमें उनके साथ मनुष्य के व्यक्तिगत सम्बन्ध का कोई भाव न था। माता जी अपने एक विशिष्ट एवं गूढ़ स्वरूप में भी प्रकट होती हैं। किसी दिव्य व्यक्ति के रूप में माता जी का यह गूढ़ स्वरूप व्यक्त होता है। माता जी स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होती हैं, इस गुप्त रहस्य का ज्ञान साधक को परमात्मा अथवा माता सरस्वती की कृपा से ही होता है।
शिष्य के लिए गुरु माता जी की विद्या माया तथा विद्या-शक्ति का प्रत्यक्ष प्राकट्य है। साधक के लिए सद्गुरु माता जी का ही स्वरूप है। साधक ने जिस आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने मार्ग-दर्शक तथा गुरु के रूप में स्वीकार किया है, वह उसके लिए भगवती माता जी का साक्षात् साकार स्वरूप है, ऐसा उसे पूर्णतम भाव से मानना चाहिए। माता जी की इस भावना के आधार के ऊपर ही साधक के आध्यात्मिक जीवन का प्रासाद स्थित होता है। हिन्दू-संस्कृति का सम्पूर्ण तत्त्व-ज्ञान इस प्रकार की भावना पर ही निर्भर करता है। यह एक अपूर्व भावना है जिसकी समता संसार की किसी भी अन्य संस्कृति में नहीं मिलती।
सद्गुरु के व्यक्तित्व में परब्रह्म का दर्शन ही साधक की आध्यात्मिक खोज की सफलता का मूल आधार है। इस प्रकार साधक-वर्ग ने जिस व्यक्ति-विशेष की शरण में जा कर उसे अपने हृदय के अन्तरतम प्रकोष्ठ में अपने आध्यात्मिक मार्ग-दर्शक के रूप में स्वीकार किया है, उसके लिए वही सद्गुरु साक्षात् पराशक्ति का स्वरूप है। वह ब्रह्मा है, वह विष्णु है, वह महेश्वर है, वह शक्ति है और वही स्वयं अक्षर परब्रह्म है। शाश्वत सत्ता की खोज में सद्भावपूर्वक तत्पर किसी भी साधक को इस सत्य को एक क्षण के लिए भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए, न विलग करना चाहिए और न उसे विस्मृत ही करना चाहिए।
साधक की दृष्टि के समक्ष गुरु का मानव-स्वरूप नहीं, वरन् उसके स्थान में परब्रह्म का तेजोमय साकार स्वरूप उपस्थित होना चाहिए। समग्र विश्व के साधकों तथा जिज्ञासुओं से चाहे वे पूर्व के हों अथवा पश्चिम के, मेरी यह विनम्र सूचना तथा विनती है। चाहे व्यक्ति किसी का भी अनुयायी हो, परन्तु एक बार अपने अन्तःकरण में किसी को सद्गुरु रूप में स्वीकार करने के पश्चात् उसके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, इस विषय में भी मेरी यह साधारण-सी सूचना है।
सद्गुरु के जीवन्त व्यक्तित्व में पराशक्ति माता जी का शुद्ध विद्या माया-स्वरूप ही व्यक्त हो रहा है-यह भावना जितनी ही अधिक दृढ़ होगी, उतनी ही मात्रा में हमारी आन्तर चेतना में दिव्य ज्ञान जाग्रत होगा तथा उतनी ही मात्रा में आत्म-साक्षात्कार में हमें सफलता प्राप्त होगी। अतः अपने सद्गुरु के चरण-कमलों की शरण स्वीकार करने वाले प्रत्येक साधक तथा शिष्य को स्मरण कराया जाता है कि उन्हें गुरु-भगवान् का पूजन करना चाहिए। सभी साधक जिन श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करते हैं, उनमें इस महागुह्य रहस्य तथा परम सत्य का निर्देश किया गया है :
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ।।
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ।।
त्वंहि विष्णुर्विरंचिस्त्वं त्वंच देवो महेश्वरः ।
त्वमेव शक्तिरूपोऽसि निर्गुणस्त्वं सनातनः ।।'
गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है और महेश्वर है गुरुदेव ।
अतः दण्डवत् गुरुदेव को परब्रह्म साक्षात् गुरुदेव ।।
गुरुमूर्ति ध्यान-मूल है गुरुपद हैं पूजा के मूल ।
मन्त्रमूल सम गुरु-वाक्य है गुरु कृपा है मोक्ष का मूल ॥
आप विष्णु हैं आप हैं ब्रह्मा आप ही देव महेश्वर हैं।
शक्तिरूप सम आप ही शोभित निर्गुण शाश्वत ईश्वर हैं।।
गुरु का सत्य स्वरूप क्या है? उनके किन स्वरूपों का हमें अनुभव करना चाहिए?
यस्यान्तर नादि मध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रम् ।
नो जातिनैव वर्णो न भवति पुरुषो नो नपुंसो न च स्त्री ।।
नाकारं नो विकारं न हि जनि मरणं नास्ति पुण्यं न पापम्।
नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि ।।'
नाम-गोत्र-कर-चरण-सूत्र नहि आदि-मध्य जिसके अन्तर।
जाति-वर्ण नहिं पुरुष नपुंसक नहि स्त्री का है अन्तर ।।
कर्म विकार जन्म-मरण नहि पुण्य-पाप से जो निर्लेप।
सहज समरस नमः सद्गुरु तत्त्व नहीं पर तत्त्व है एक ।।
दिव्य विद्या माया के व्यक्त स्वरूप के महान् रहस्य का स्वल्प विवरण इस पवित्र स्तवन में हमें देखने को मिलता है।
महान् धर्मशास्त्रों का सारतत्त्व
आज विजय के गौरवपूर्ण दिवस पर विजयी विद्या-माया-स्वरूपा भगवती माता जी की हम जो आराधना कर रहे हैं, वह सद्गुरु के आध्यात्मिक व्यक्तित्व में तथा उसके द्वारा प्रकट हो रहे सर्वोपरि परब्रह्म की ही पूजा है। हमने विविध प्रकार से माता जी की आराधना की है। आज हमने धर्मग्रन्थों के पाठ द्वारा विद्यारम्भ से विशेषकर माता जी के वाङ्मय स्वरूप की आराधना करने का प्रयत्न किया है। गीता, ब्रह्मसूत्र, भागवत, रामायण इत्यादि श्रेष्ठ धर्मशास्त्र माता जी के वाङ्मय-स्वरूप है।
धर्मशास्त्रों के पाठ से माता जी के वाङ्मय स्वरूप की आराधना किस प्रकार होती है, इस विषय में यहाँ कुछ शब्द कहना अप्रासांगिक न होगा। हम देख चुके हैं कि स्वाध्याय साधक के लिए एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया है; परन्तु यह जीवन का व्यावहारिक मार्ग भी है। स्वाध्याय हमारी आकांक्षाओं, हमारे आदर्शों तथा हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारों का सुन्दर निर्माण करता है। अतएव गीता, ब्रह्मसूत्र, भागवत, रामायण तथा महाभारत जैसे धर्मग्रन्थ हमारे आध्यात्मिक जीवन में श्रेष्ठ मार्ग-दर्शन प्रदान करते हैं।
भगवद्गीता के द्वारा माता जी क्या सार प्रदान करती हैं? भगवद्गीता द्वारा माता जी का एक ही आदेश है और वह है त्याग। गीता का अर्थ है त्याग। गीता त्याग का रहस्य समझाने वाला धर्मग्रन्थ है। गीता कहती है कि इस व्यावहारिक जगत् से सम्बद्ध सम्पूर्ण पदार्थों का त्याग करना, अपने कर्तृत्व-अभिमान, अहंता और ममता का त्याग करना तथा सम्पूर्ण विश्व भगवान् का विराट् स्वरूप है और हमारे सभी कर्म उस विराट् की पूजा हैं, ऐसी दृढ़ भावना रखना ही परम तत्त्व के साक्षात्कार का एक मार्ग है। अनासक्ति और त्याग-ये दो गीता के परम आदेश हैं।
भागवत में हमें सकारात्मक पक्ष का दर्शन होता है। इस दृश्य जगत् का त्याग करो। नश्वर जगत् के सभी पदार्थों के प्रति मन का मोह दूर करो तथा परमात्मा के प्रति परम प्रेम रखो। भागवत का सम्पूर्ण सन्देश 'प्रेम' शब्द में समाहित है। यह प्रेम भगवत्प्रेम है। यह शुद्ध प्रेम का प्रोज्ज्वल सार-तत्त्व है, भगवान् के प्रति रति है। गीता पूर्ण अनासक्ति का उपदेश देती है, पर भागवत भगवच्चरण में पूर्ण हृदय से अनुरक्त होने को कहता है।
महाभारत 'धर्म' के आदर्श पर अटल बने रहने को कहता है। उसका उपदेश है कि जीवन का बलिदान दे कर भी धर्म के सिद्धान्तों से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म पर ही टिके रहो। धर्म से ही अन्तःकरण तथा जीवन निर्मल बनते हैं, पवित्र बनते हैं।
मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का आचरण कैसे शक्य होता है, यह रामायण में बताया गया है। रामायण का ग्रन्थ हमारे समक्ष एक आदर्श धार्मिक व्यक्ति के ठोस तथा व्यावहारिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श सेवक, आदर्श जिज्ञासु तथा आदर्श राजा का प्रतिमान प्रस्तुत करता है। मनुष्य-जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के आदर्शों का सच्चा दर्शन रामायण के दिव्य पात्रों के द्वारा हमें कराया गया है। यदि मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने के साथ-साथ धार्मिक जीवन यापन करना चाहता है, तो उसे अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, इसका प्रतिरूप रामायण में दिया गया है। रामायण में वर्णित प्रसंगों से शिक्षा ले कर मनुष्य परम धार्मिक जीवन यापन के अनुकूल अपने जीवन को ढाल सकता है।
ब्रह्मसूत्र में इन सभी का मूलभूत कारण दर्शाया गया है। मनुष्य-जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, उसे इसमें बतलाया गया है। यह कहता है-"अविनाशी परम तत्त्व शाश्वत आनन्द की प्राप्ति ही जीवन का ध्येय है और ये सभी पदार्थ इस ध्येय की प्राप्ति के लिए साधन हैं। इन सब साधनों से परम धाम की प्राप्ति होती है, जहाँ पहुँच कर दुःख तथा मृत्यु से संकुल इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता।" ब्रह्मसूत्र का अन्तिम मन्तव्य यह है कि धर्म, त्याग तथा भक्ति-मार्ग से एक बार परब्रह्म की प्राप्ति कर लेने के पश्चात् 'न पुनरावर्तते' अर्थात् जीव पुनः वापस नहीं आता। वह सदा-सर्वदा के लिए असीम चेतना, अविनाशी सत्ता, शाश्वत आनन्द तथा चिरन्तन शान्ति में अवस्थित हो जाता है।
यही ध्येय है। 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम' - ऐसा भगवान् गीता में कहते हैं। इस परम धाम में पहुँच कर मनुष्य पुनः इस संसार में वापस नहीं आता।
यही परम परिपूर्णता का स्वरूप है। 'यो वै भूमा तत्सुखम्।' यह भूमा ही इस जगत् में मनुष्य का ध्येय है।
जिसके जान लेने पर अन्य कुछ जान लेने को शेष नहीं रहता- 'यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति।" (जान कर फिर जानना रहता न कुछ भी शेष है।)
जिसको प्राप्त कर लेने पर अन्य कोई प्राप्तव्य नहीं रहता- 'यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।' (प्राप्त कर जिसको कि कुछ पाना न रहता शेष है।)
जिसकी प्राप्ति तथा अनन्त उपभोग के लिए हम यहाँ निरन्तर प्रयास कर रहे हैं, ऐसी अलौकिक स्थिति की महिमा का, उसके परम ऐश्वर्य का वर्णन है। इस भाँति वे हमें ध्येय तथा आदर्श दोनों ही प्रदान करते हैं। आत्म-साक्षात्कार हमारा ध्येय है। इनके साधन हैं गीता में वर्णित त्याग, भागवत में बतायी गयी भक्ति, महाभारत का धर्म तथा रामायण का आदर्श जीवन।
मनुष्य-जीवन का लक्ष्य तथा उद्देश्य तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट तथा गम्भीर रूप इन श्रेष्ठ धर्मग्रन्थों में से जानने को मिलता है। यदि कोई साधक इन साधनों द्वारा ध्येय के प्राप्त्यर्थ प्रयास करने में तत्पर हो, तो उसके लिए व्यावहारिक सूचना भी प्राप्त होती है।
प्रार्थना
परमा माता भगवती की नवरात्र के नौ दिन की आराधना के अन्त में आने वाले इस विजयादशमी के महोत्सव में हम उनसे प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदय में बुद्धि तथा स्मृति-रूप में प्रकट हों। हम सब माता जी से प्रार्थना करें कि वह स्मृति-रूप में इन महान् सत्यों को हमारे हृदय में सदा सजीव बनाये रखें जिन पर हमारा सम्पूर्ण जीवन आधारित हो और जिसके आधार पर हमारे समस्त जीवन का गठन हो तथा इन महान् सत्यों को हम जीवन में चरितार्थ करें; क्योंकि उनकी 'भ्रान्ति-शक्ति' तथा 'माया-शक्ति' इतनी रहस्यमयी हैं कि हम इन सत्यों से सुपरिचित हैं, हम उनके विषय में बारम्बार सुनते हैं और इससे हम उन्हें स्मरण रखने का प्रयास करें, तो भी न जाने कैसे एक पल में वह हमें विस्मृत करा देती हैं और इस वैषयिक जगत् की इन बाह्य वस्तुओं का ही बोध कराती हैं। हमारी चेतना के ऊपर माता जी का यह आवरण पड़ते ही एक क्षण में ही इन महान् सत्यों को हम भूल जाते हैं। हम क्षणिक आनन्द प्रदान करने वाले पदार्थों में ही तन्मय बन जाते हैं और बाह्य जगत् के नाम-रूपों में बंध जाते हैं। अतः हम बार-बार प्रार्थना करें-"हे माँ! विद्या-स्वरूप में हमारे पास प्रकट हों। तुम्हारे विद्या-स्वरूप से हमारी चेतना प्रकाशित हो।"
देवीसूक्त का पाठ करते समय अभी हमने देखा कि माता जी ही सब-कुछ हैं। निद्रा, क्षुधा, छाया, तृष्णा, भ्रान्ति इत्यादि माता जी के ही स्वरूप हैं। इसके साथ ही वह बुद्धि, दया आदि भी हैं। अतः हमें करबद्ध तथा नतमस्तक हो कर प्रार्थना करनी चाहिए- "हे माँ! तुम अपने तेजोमय स्वरूप से मुझमें प्रकट होओ और अपने अविद्या माया-स्वरूप से मेरी रक्षा करो।" माता जी प्रसन्न होंगी, वह तुष्ट होंगी और अपने तेजोमय नेत्रों से हमें देखेंगी, हमारे सामने मन्द स्मित करेंगी। तब हमारी समस्त भ्रान्ति, सम्पूर्ण दुःख, समग्र अन्धकार का अन्त होगा और हम माता जी के सच्चिदानन्द परब्रह्म-स्वरूप का दर्शन पायेंगे।
इन दस दिनों में हमने माता जी के रूप के बाह्य छोर का ही स्पर्श करने का प्रयास किया। माता जी के स्वरूप का अणु मात्र ही समझ सकें, इसके लिए हमने प्रयत्न किया। हम अनन्त काल तक घण्टों तक बोलते रहें, तब भी माता जी के अगम्य स्वरूप का रंच मात्र भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकेगा। सर्भ। धर्मग्रन्थ तथा सभी सन्त अनन्त काल से माता जी का वर्णन करते आ रहे हैं, फिर भी वह अभी तक अपूर्ण ही है। माता जी ने जिस परिधान से अपने को आवृत कर रखा है, उसके छोर मात्र का ज्ञान हमें इन अल्प शब्दों द्वारा हुआ है, ऐसा मानना हमारी धृष्टता ही होगी। हम तो केवल राई के दाने के बराबर ही उनका ज्ञान प्राप्त कर सके हैं।
माता जी के विषय में जो जानना शेष रहा है, वह महासागर के विशाल तट की बालुका के समान है। बाल-सुलभ प्रेम ही माता जी के पास बालकों को ले जाता है और उन्हें जानने तथा उनका हाथ पकड़ने के प्रयास में समर्थ बनाता है। इन दस दिनों में हमने जो माता जी के सम्बन्ध में चर्चा करने का प्रयास किया है, वह उनके जानने के लिए नहीं किया है। यदि माता जी स्वयं कृपा कर अपने को प्रकट करें, तभी हम उन्हें जानने की आशा कर सकते हैं। यह तो मात्र उनके चरण कमलों में पुष्प अर्पण करने का एक नम्र प्रयास था
इन नौ दिनों में माता जी की विविध प्रकार से पूजा की गयी। आराधना में भजन, कीर्तन, नृत्य, अलंकार, पूजा इत्यादि थे तथा पूजा के अंग के रूप में माता जी द्वारा प्रदान की हुई वाणी से उनकी 'वाक्शक्ति' के स्वरूप का हमने पूजन किया व हमने शब्दों द्वारा उनकी आराधना करने का प्रयास किया। इस विजयादशमी के पवित्र दिवस पर माता जी के चरण कमलों में ये अल्प शब्द अर्पित कर प्रार्थना करते हैं- "हे माँ, यह अल्प भी स्वीकार करो। तू प्रेम है। तू करुणा है। तू प्रकाश है। तू मुक्ति है। यह सब कहने का क्या तात्पर्य है? इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हे माँ, तू माँ है। अतः माँ-रूप में तुम्हारे चरणों में अर्पित प्रेम की यह भेंट स्वीकार करो और हम पर अपनी कृपा की वृष्टि करो। हमारी ओर मुस्कानपूर्ण दृष्टिपात कर अपनी अविद्या माया का अन्धकार विदूरित कर दो। हमारे गुरुदेव के दिव्य चरणों में रहने वाले सभी साधकों को आत्मज्ञान-रूपी तेजोमय प्रकाश तथा सच्चिदानन्द का अक्षय सुख प्रदान करो।”
परिशिष्ट
श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती (जीवन-झांकी)
पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द के योग्य आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री स्वामी चिदानन्द के विषय में कहा गया है-"यदि कोई कृश काया के पीछे छिपे आत्मवीर को सौम्य चेहरे के पीछे छिपे नियन्त्रित हृदय को, कर्म की गतिशीलता के पीछे छिपी गहन मानसिक शान्ति को तथा व्यक्तिगत स्तरीय प्रेम-परिचर्या के पीछे छिपी निवैयक्तिक अनामक्ति का दर्शन करना चाहता है, तो उसे स्वामी चिदानन्द से भेंट करती चाहिए।"
स्वामी चिदानन्द ने दक्षिण भारत के एक समृद्ध परिवार में २४ सितम्बर १९१६ को जन्म लिया था। प्रारम्भ से ही परम्पराओं और कर्मकाण्डों में उनकी रुचि थी। मद्रास (चेन्नै) स्थित लोयोला फालेज के वह एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन पर जेसस क्राइस्ट के आदशों और उपदेशों की बहुत गहरी छाप पड़ी। उन्होंने हिन्दू-संस्कृति के तत्त्वों के साथ उनका समन्वय कर लिया। श्री रामकृष्ण तथा अपने गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द से वह अत्यधिक प्रभावित रहे। वर्ष १९४३ में वह गुरुदेव की शरण में आ गये। तबसे उनके गुरुदेव का आश्रम उनका घर बन गया तथा द डिवाइन लाइफ सोसावटी के महान आदर्श उनके सेवा-कार्यों की आधारशिला बन गये।
प्रारम्भ से ही स्वामी चिदानन्द में रोगियों और दुःखी व्यक्तियों की सेवा करने का अतीव उत्साह था। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अपने घर के लॉन में कुष्ठियों के लिए झोपड़ियाँ निर्मित करवा दी थी और उन्हें देव-तुल्य मान कर वह उनकी परिचर्या किया करते थे।
अपने आध्यात्मिक पुत्र तथा प्रिय शिष्य स्वामी चिदानन्द के विषय में स्वामी शिवानन्द ने कहा था- "चिदानन्द जीवन्मुक्त, महान् सन्त, आदर्श योगी तथा परा भक्त हैं। इसके अतिरिक्त भी वह बहुत कुछ हैं। अपने पिछले जन्म में वह एक महान् योगी तथा सन्त थे। उनके प्रवचन उनके पवित्र हृदय के भावोद्गार तथा उनकी प्रातिभज्ञानात्मक प्रज्ञा के प्रकटीकरण हैं। वह एक व्यावहारिक वेदान्ती हैं। उनके शब्दों में अद्भुत प्रभावक शक्ति है। एक महान् मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है।"
एक उत्कृष्ट संन्यासी के रूप में आध्यात्मिक चुम्बकत्व के गुण के धनी स्वामी जी अनगिनत व्यक्तियों के प्रियपात्र बन गये तथा संसार-भर में दिव्य जीवन के महान् आदशों के पुनरुजीवन के लिए सभी दिशाओं में कठिन परिश्रम करते-करते अन्ततः २८ अगस्त २००८ को ब्रह्मलीन हो गये।