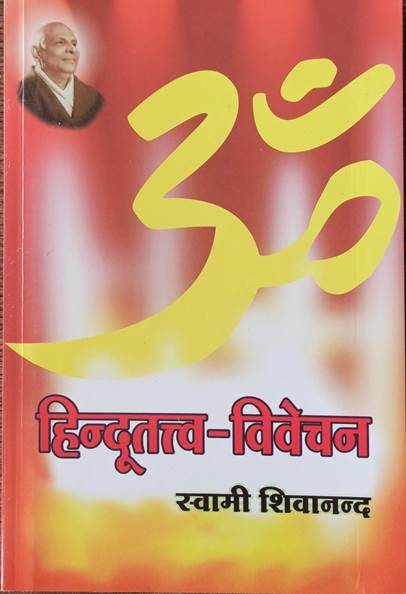
हिन्दूतत्व-विवेचन
ALL ABOUT HINDUISM
का हिन्दी अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी शिवानन्द समर्पण
अनुवादिका
डा. स्वर्णलता अग्रवाल
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण : २०००
द्वितीय हिन्दी संस्करण: २००७
तृतीय हिन्दी संस्करण : २०१७
(१,००० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
HS 292
PRICE: 160/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए
स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त
फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर, जि. टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड,
पिन २४९ १९२ में मुद्रित ।
For online orders and Catalogue visit: disbooks.org
|
समर्पण
उन सबको- जिन्हें हिन्दूतत्त्व तथा इसके उदात्त दर्शन से प्रेम है और जो इसकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं !
|
प्रकाशकीय
हिन्दू-धर्म वस्तुतः समस्त धर्मों का स्रोत है। इसमें सभी धर्मों का बीज समाहित है। इसमें समस्त धर्मों का समावेश है, कोई भी धर्म इसकी परिधि से बाहर नहीं है।
सार्वभौमिक स्तर पर प्रभावकारी इस हिन्दूतत्त्व के प्रति जगत् के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक ही है।
यह पुस्तक हिन्दूतत्त्व-रूपी स्फटिक के विभिन्न पहलुओं से परिचित होने की जिज्ञासा रखने वाले पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस पुस्तक का अँगरेजी संस्करण सर्वप्रथम सन १९४७ में 'ऑल अबाउट हिन्दूइज्म' (All About Hinduism) नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत पुस्तक सन् १९९३ में प्रकाशित इसके पाँचवें परिवर्धित संस्करण का हिन्दी अनुवाद है।
हम आशा करते हैं कि हिन्दूतत्त्व तथा इसके दार्शनिक पक्षों में रुचि रखने वाले हिन्दी भाषा-भाषी पाठकों के लिए यह हिन्दी संस्करण रुचिकर तथा उपयोगी सिद्ध होगा।
-द डिवाइन लाइफ सोसायटी
विश्व-प्रार्थनाएँ
१
हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव!
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है।
तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ हो ।
तुम सच्चिदानन्दघन हो ।
तुम सबके अन्तर्वासी हो।
हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समत्व प्रदान करो।
श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो।
हमें आध्यात्मिक अन्तःशक्ति का वर दो,
जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों।
हम अहंकार, काम, लोभ, घृणा, क्रोध और द्वेष से रहित हों।
हमारा हृदय दिव्य गुणों से परिपूरित करो।
हम सब नाम-रूपों में तुम्हारा दर्शन करें।
तुम्हारी अर्चना के ही रूप में इन नाम-रूपों की सेवा करें।
सदा तुम्हारा ही स्मरण करें।
सदा तुम्हारी ही महिमा का गान करें।
तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे अधर-पुट पर हो।
सदा हम तुममें ही निवास करें ।
२
हे अदृश्य प्रभु! हे आराध्य देव! हे परमेश्वर! आप अनन्त आकाश से ले कर घास के छोटे-से तिनके तक इस असीम विश्व में व्याप्त हैं। आप मेरी आँखों के तारे हैं, मेरे हृदय के प्रेम हैं। मेरे जीवन के प्राण हैं; मेरे आत्मा के दिव्य तत्त्व हैं; मेरी बुद्धि तथा इन्द्रियों के प्रदीपक हैं; मेरे हृदय के मधुर अनाहत संगीत हैं और मेरे स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों के आधार हैं।
मैं एकमात्र आपको ही इस विश्व के सर्वशक्तिमान् शासक और मेरे तीनों शरीरों का अन्तर्यामी मानता हूँ। मेरे प्रभु! मैं आपको बारम्बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप ही मेरे एकमात्र आश्रय तथा अवलम्ब हैं। मेरी आस्था आप ही पर केन्द्रित है। हे प्रेम और करुणा के सागर! मेरा उत्थान करें! मुझे प्रबुद्ध करें! मेरा मार्ग-दर्शन करें तथा मेरी रक्षा करें! मेरे आध्यात्मिक पथ की बाधाएँ दूर करें तथा अज्ञानावरण को विदूरित करें! हे जगद्गुरु! मैं इस जीवन के, इस देह के और इस संसार के कष्ट एक क्षण के लिए भी अब और अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूँ। हे प्रभु! शीघ्र दर्शन दें! मैं आपके लिए लालायित हूँ, मैं द्रवित हो चला हूँ। मेरी भाव-प्रवण, आन्तरिक प्रार्थना सुनें, सुनें। निष्ठुर न बनें, मेरे स्वामी! आप दीनबन्धु हैं, अधम उद्धारक हैं, पतितपावन हैं।
३
सर्वेषां स्वस्ति भवतु ।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु ।
सर्वेषां पूर्ण भवतु ।
सर्वेषां मंगलं भवतु ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत् ।।
असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
विषय-सूची
हिन्दूतत्त्व पर एक विहंगम दृष्टि
'हिन्दू' शब्द का उद्भव और महत्त्व
हिन्दू-धर्म की उत्तरजीविता के कारण
आचार-नीति अर्थात् आचरण-विज्ञान
आचार-नीति, आध्यात्मिकता और धर्म
आचार-नीति का अभ्यास करने के लाभ
हिन्दू-धर्म में आचार-नीति की संहिताएँ
हिन्दू-आचार-नीति के मौलिक सिद्धान्त
आचार-नीति के संवर्धन अथवा शोधन की प्रक्रिया
नवरात्र या नौ-दिवसीय देवी-पूजन
मूर्ति-पूजा का दर्शन तथा महत्त्व
कर्मकाण्डीय (वैधी) भक्ति से परा-भक्ति की ओर
हिन्दू-दर्शन की महिमा तथा हिन्दू-पूजा-पद्धति
हिन्दू-धर्मविज्ञान-विषयक वर्गीकरण
दर्शन : इसका उद्भव तथा इसकी सीमाएँ
भारतीय दर्शन की शास्त्रसम्मत तथा शास्त्रविरुद्ध शाखाएँ
षड्-दर्शन अथवा छह शास्त्रसम्मत मतवाद
श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत-दर्शन
श्री मध्वाचार्य का द्वैत-दर्शन
श्री निम्बार्क का द्वैताद्वैत-दर्शन
श्री वल्लभ का शुद्धाद्वैत-दर्शन
श्री चैतन्य का अचिन्त्य-भेदाभेद-दर्शन
धर्म की सेवा का सुयोग्य अधिकारी कौन है?
राष्ट्र के संगठन के लिए आह्वान
भगवद्गीता : भारतीय संस्कृति की आधारशिला
प्रथम अध्याय
हिन्दूतत्त्व पर एक विहंगम दृष्टि
सच्चिदानन्द को मौन प्रणाम जो समस्त मनों का मौन साक्षी है; जो अन्तर्यामी है; जिसने अपनी लीला के लिए इस विश्व को रचा है; जो इस विश्व का, शरीर और मन का तथा समस्त गतिविधियों का आश्रय है तथा जो समस्त संगठनों एवं उनके कार्यकलापों का आधार है।
धर्म का उद्देश्य
धर्म को अँगरेजी भाषा में 'रिलीजन' (Religion) कहते हैं। रिलीजन लैटिन शब्द 'रेलिजिओ' से बना है। 'रेलिजिओ' में दो शब्द हैं-'रि' (पीछे) तथा 'लिगेअर' (लाना या बाँधना)। जो आत्मा को परमात्मा से पुनः बाँध देता या सम्बद्ध कर देता है, वह धर्म है। धर्म ईश्वर-साक्षात्कार का मार्ग दर्शाता है।
धर्म उन मानवों की गहन आन्तरिक आकांक्षा की पूर्ति करता है जो केवल पशुओं के समान जीवन-यापन करने मात्र से सन्तुष्ट नहीं होते तथा आध्यात्मिक आश्वासन, आश्रय और शान्ति चाहते हैं। मनुष्य केवल रोटी पर जीवित नहीं रह सकता। हममें से बहुतों के जीवन में एक समय आता है जब केवल सांसारिक सुखों से सन्तुष्ट न हो कर हम 'कुछ और' के लिए छटपटाते हैं। कई लोगों के जीवन में विपत्तियाँ और परेशानियाँ उनका ध्यान आध्यात्मिकता से प्राप्त होने वाली सान्त्वना की ओर प्रवृत्त कर देती हैं।
हिन्दू-धर्म की विशेषताएँ
एक अपौरुषेय धर्म
हिन्दू-धर्म सार्वभौमिक धर्म है जो भारत में सर्वाधिक प्रचलित हुआ। यह समस्त जीवन्त धर्मों में प्राचीनतम है। यह किसी धर्मप्रवर्तक के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। ईसाई, बौद्ध और इस्लाम धर्मप्रवर्तकों द्वारा चलाये गये थे। उनके उद्भव की तिथियाँ निश्चित हैं; परन्तु हिन्दू-धर्म के लिए ऐसी कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। प्रवर्तकों के उपदेशों से हिन्दू-धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई; यह विशिष्ट गुरुओं द्वारा बताये हुए विशिष्ट सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है। यह धार्मिक मतान्धता से मुक्त है।
हिन्दू-धर्म को सनातन-धर्म तथा वैदिक-धर्म भी कहते हैं। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म। हिन्दू-धर्म उतना ही प्राचीन है जितना कि संसार। हिन्दू-धर्म सब धर्मों का जन्मदाता है। हिन्दू-धर्म-ग्रन्थ विश्व के प्राचीन ग्रन्थ हैं। हिन्दू-धर्म को केवल शाश्वत होने के कारण ही सनानत-धर्म नहीं कहा जाता, प्रत्युत् इसलिए भी कि यह ईश्वर द्वारा रक्षित है और यह हमें शाश्वत बना सकता है।
वैदिक-धर्म का अर्थ है वेदों का धर्म। वेद हिन्दू-धर्म के आधारभूत ग्रन्थ हैं। भारत के प्राचीन ऋषि-मुनियों ने उपनिषदों में अपनी अन्तर्शात आध्यात्मिक (अपरोक्ष) अनुभूतियाँ व्यक्त की हैं। ये अनुभव साक्षात् और अचूक हैं। हिन्दू-धर्म में पुरातन ऋषियों की इन अनुभूतियों को अपनी प्रामाणिकता का आधार माना जाता है। अनादि काल से हिन्दू ऋषि-मुनियों द्वारा प्राप्त अमूल्य सत्य हिन्दू-धर्म का गौरव हैं; अतएव हिन्दू-धर्म एक अपौरुषेय धर्म है।
स्वतन्त्रता का धर्म
हिन्दू धर्म में यह दुराग्रह नहीं है कि केवल इसी के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी धर्म के द्वारा नहीं। यह ध्येय के लिए साधन मात्र है और सभी साधन जो अन्ततः एक लक्ष्य पर ले जाते हैं, वे समान रूप से मान्य हैं।
हिन्दू-धर्म मनुष्य के विवेकशील मस्तिष्क को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता है। यह मानवीय तर्क की तथा मानव के विचार, भाव और आकांक्षा की स्वतन्त्रता पर अनुचित रोक नहीं लगाता। और उपासना के क्षेत्रों में यह सर्वाधिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। हिन्दू-धर्म स्वतन्त्रता का धर्म है। ईश्वर की प्रकृति, आत्मा, सृष्टि, उपासना का रूप और जीवन का लक्ष्य आदि प्रश्नों के सम्बन्ध में यह मानवीय तर्क और हृदय को पूर्ण स्वतन्त्रता देता है। सिद्धान्त विशेष की स्वीकृति अथवा कोई विशेष कर्मकाण्ड अथवा उपासना हिन्दू-धर्म नहीं है। यह विशेष सिद्धान्तों या उपासना के विशिष्ट रूपों को स्वीकार करने के लिए किसी को विवश नहीं करता। यह प्रत्येक व्यक्ति को चिन्तन करने, अनुसन्धान करने और विचार करने की स्वतन्त्रता देता है। अतएव सब प्रकार की धार्मिक आस्थाएँ, उपासना या साधना के विभिन्न रूप, कर्मकाण्ड एवं रीतिरिवाजों के अनेक प्रकार-सभी को हिन्दू धर्म में साथ-साथ सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ है और सभी में पारस्परिक सद्भावपूर्ण सम्बन्ध रहा है। इसी रूप में वे संस्कृत एवं विकसित हुए हैं।
जो व्यक्ति ईश्वर को सृष्टिकर्ता और शासक नहीं मानते, जो शाश्वत आत्मा के अस्तित्व अथवा मोक्ष की स्थिति को स्वीकार नहीं करते, हिन्दू-धर्म उनकी उपेक्षा नहीं करता। हिन्दू-धर्म ऐसे विचार वालों को भी हिन्दू-धर्म-समाज के सम्माननीय सदस्य मानता है।
हिन्दुओं का धार्मिक आतिथ्य लोकप्रसिद्ध है। हिन्दू धर्म अत्यन्त उदार है। यह हिन्दू-धर्म की मौलिक विशिष्टता है। हिन्दू-धर्म समस्त धर्मों का मान करता है। वह किसी अन्य धर्म से द्वेष नहीं करता। वह सत्य का किसी भी स्वरूप में मान करता है और उसे स्वीकार करता है।
भारत में अन्य धर्मों के अनुयायी प्रचुर संख्या में हैं; तथापि हिन्दू लोग उन सबके साथ सद्भाव, शान्ति और मित्रता से रहते हैं। अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ उनकी सहिष्णुता और सौहार्दभाव सराहनीय हैं।
तात्त्विक सिद्धान्तों, धार्मिक अनुशासन के ढंगों, कर्मकाण्ड की क्रियाओं एवं हिन्दू-समाज में प्रचलित सामाजिक आदतों में भेद होते हुए भी हिन्दुओं के समस्त वर्गों में धर्म की संकल्पना और जीवन तथा जगत् के प्रति दृष्टिकोण में एक अनिवार्य समानता है।
योग और वेदान्त की महिमा
वेदान्त (अथवा उपनिषदों का दर्शन) उच्च, उत्कृष्ट तथा असाधारण है। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी उपनिषदों के ऋषि-मनीषियों के प्रति सम्मान प्रकट किया है। वे उनके व्यक्तित्व की ऊँचाइयों को देख कर चकित रह गये हैं। शोपेनहावर नित्य उपनिषदों का अध्ययन करते और सोने से पूर्व उनमें निहित विचारों पर मनन करते थे। उन्होंने कहा है- "उपनिषद् मेरे जीवन में सान्त्वना के स्रोत हैं और वे मुझे मृत्यु के उपरान्त भी शान्ति प्रदान करेंगे।"
हिन्दू-धर्म में राजयोग की पद्धति विशिष्ट एवं अनुपम है। उसके उपदेश अत्यन्त व्यावहारिक और शिक्षाप्रद हैं। विश्व की कोई भी शारीरिक व्यायाम की विद्या हठयोग से प्रतियोगिता नहीं कर सकती। कुण्डलिनीयोग अद्भुत है। इसी कारण अमरीका और यूरोप के निवासी हिन्दू-संन्यासियों एवं योगियों की खोज में रहते हैं। वे बहुधा योग-शिक्षकों की खोज में हिमालय जाते हैं। कुछ तो हिन्दू-योगियों के शिष्य बन योगाभ्यास कर रहे हैं। यूरोप और अमरीका के अधिकांश लोग अब भी विश्वास और अभ्यास से हिन्दू हैं, यद्यपि वे जन्म से ईसाई हैं। वे राजयोग और वेदान्त का अभ्यास करते हैं।
अभ्यास पर बल
हिन्दू-धर्म में सब प्रकार के लोगों के लिए उनके स्वभाव, सामर्थ्य, रुचि, आध्यात्मिक विकास के स्तर तथा जीवन की परिस्थितियों के अनुसार आध्यात्मिक भोजन एवं योग-साधना की व्यवस्था है। अपना सामान्य व्यवसाय करने वाले मेहतर और मोची तक के लिए आत्मसाक्षात्कार हेतु योग साधना बतलायी गयी है। हिन्दू योग और वेदान्त के शिक्षक आत्म-संयम, तप, वैराग्य और व्यावहारिक साधना पर विशेष बल देते हैं; क्योंकि इनसे मन और इन्द्रियों पर नियन्त्रण प्राप्त करने, दिव्य शक्तियों को प्रकट करने अथवा आत्मसाक्षात्कार करने में बहुत सहायता मिलती है। हिन्दू-धर्म मात्र सिद्धान्तों का धर्म नहीं है। यह मुख्य रूप से व्यावहारिक है। किसी अन्य धर्म में आपको व्यावहारिक योग की इतनी विविधता और इतना उत्कृष्ट असाधारण दर्शन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि भारत ही सन्तों, ऋषियों, योगियों और साधुओं की महान् भूमि रहा है।
धर्म दर्शन का व्यावहारिक स्वरूप है। दर्शन धर्म का बुद्धिसंगत पक्ष है। हिन्दू-धर्म का दर्शन सुगम दर्शन नहीं है। यह बौद्धिक उत्सुकता शान्त करने और व्यर्थ के वाद-विवाद के लिए भी नहीं है। हिन्दू-दर्शन जीवन की एक शैली है। हिन्दू-दार्शनिक श्रुतियों को सुन कर गम्भीरता से मनन करता है, आत्मविचार करता है, निरन्तर ध्यान करता है और तब आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करता है। उसका लक्ष्य मोक्ष होता है। वह अभी और यहीं जीवन्मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है।
एक हिन्दू के लिए धर्म मानव-जीवन का अध्यात्मीकरण है। उसके लिए धार्मिक संस्कृति ही वास्तविक स्वतन्त्रता की संस्कृति है। धर्म हिन्दू-जीवन के समस्त पक्षों का संचालन करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव को आत्मा की स्वतन्त्रता की अनुभूति प्राप्त कर लेनी चाहिए। वास्तविक स्वतन्त्रता की संस्कृति हेतु सर्वाधिक अवसर धर्म में ही निहित है। जीवन में पूर्ण स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए धर्म ही एकमात्र साधन है।
केवल भारतवर्ष में ही ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन के विषय में न्यूनाधिक ज्ञान है। पशुओं को चराने वाला ग्वाला, खेतों में हल चलाने वाला किसान, नाव चलाने वाला नाविक भी दार्शनिक सत्यों को प्रकट करने वाले गीत गाता है। नाई तक अपना उस्तरा उठाने से पूर्व 'ॐ नमः शिवाय', 'शिवोऽहम्' आदि मन्त्रों का उच्चारण करता है। परमहंस संन्यासियों (जो हिन्दू-धर्म के भ्रमणशील सन्त रहे हैं) ने घर-घर जा कर सर्वोच्च वेदान्त की शिक्षा का प्रचार किया है। मुट्ठीभर चावल के बदले में उन्होंने धार्मिक गीतों के माध्यम से हिन्दू धर्म और दर्शन के हीरे मोती घर-घर बाँटे हैं।
हिन्दू कौन है ?
सनातनधर्म-सभा की एक गोष्ठी में लोकमान्य तिलक ने कहा था- जो यह मानता है कि वेदों में स्वयंसिद्ध और स्वतः प्रमाण सत्य निहित हैं, वह हिन्दू है।"
हिन्दू महासभा ने एक और परिभाषा दी है- "जो व्यक्ति भारतवर्ष में उद्भूत धर्म में विश्वास करता है, वह हिन्दू है।"
कुछ लोगों के अनुसार- "जो मृतक का दाहसंस्कार करते हैं, वे हिन्दू हूँ।" एक अन्य परिभाषा के अनुसार- "हिन्दू वह है जो गौ और ब्राह्मण की रक्षा करता है।"
कुछ कहते हैं-"भारत को अपनी मातृभूमि और पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान मानने वाले हिन्दू हैं।"
अन्य कुछ लोग कहते हैं-"जो व्यक्ति अपने-आपको हिन्दू मानता और कहता है, वह हिन्दू है।"
कुछ लोग परिभाषा करते हैं- "जो व्यक्ति वेदों, स्मृतियों, पुराणों और तन्त्रों को धर्म का मूल एवं आचरण के नियमों का आधार मानता है तथा एकमात्र परब्रह्म, कर्म के सिद्धान्त अथवा प्रतिफलात्मक न्याय एवं पुनर्जन्म में आस्था रखता है, वह हिन्दू है।"
"जो वैदिक अथवा सनातन धर्म का अनुयायी है, वह हिन्दू है।" यह एक अन्य परिभाषा है।
"वेदान्त का अनुयायी हिन्दू है।" यह भी हिन्दू की एक परिभाषा है।
कुछ सुसंस्कृत विद्वानों के अनुसार- "कर्म के सिद्धान्त, पुनर्जन्म, अवतार, पितृ-पूजा, वर्णाश्रम-धर्म, वेद, ईश्वर के अस्तित्व में जिसे पूर्ण विश्वास है, जो वेदों की शिक्षाओं को पूर्ण आस्था से और मन लगा कर व्यवहार में लाता है, जो सन्ध्या, श्राद्ध, पितृ-तर्पण और पंचमहायज्ञ करता है, जो वर्णाश्रम-धर्म का पालन करता है, जो अवतारों की उपासना करता और वेदों का अध्ययन करता है, वह हिन्दू है।"
यही परिभाषा पूर्ण तथा सही है।
'हिन्दू' शब्द का उद्भव और महत्त्व
महान् आर्य-प्रजाति का वह समूह जो दरों के मार्ग से मध्य एशिया से भारत में आया, सर्वप्रथम सिन्धु नदी के पास के जनपदों में बस गया था। पारसी लोग 'सिन्धु' शब्द का उच्चारण 'हिन्दू' करते हैं और वे अपने आर्य भाइयों को 'हिन्दू' कह कर पुकारने लगे। हिन्दू सिन्धु का अपभ्रंश है।
हिन्दू आर्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में फैल गये, तब पारसियों ने पंजाब और वाराणसी के बीच के समस्त क्षेत्र को 'हिन्दुस्तान' (हिन्दुओं के रहने का स्थान) नाम दे दिया।1
संस्कृत-साहित्य में प्रयुक्त हिन्दुस्तान का प्राचीन नाम है भारतवर्ष अथवा भरतखण्ड। यह नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। भरत प्राचीन काल में एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन करता था। मनु ने समस्त केन्द्रीय हिमालय और विन्ध्य पर्वतों के मध्य के भाग को 'आर्यावर्त' (अर्थात् आर्यों का निवास-स्थान) नाम दिया। सम्पूर्ण भारत के लिए एक दूसरा नाम है जम्बूद्वीप। ग्रीक लोगों ने इस समूचे देश को 'इंडु' नाम दिया; इसी कारण समस्त यूरोप में 'इंडिया' नाम प्रसिद्ध हो गया।
'हिन्दू' शब्द मात्र नाम नहीं है। 'हिन्दू' नाम केवल केवल भौगोलिक महत्त्व का ही नहीं है, वरन् राष्ट्रीय और प्रजातीय महत्त्व का है। आरम्भ से ही हमारे राष्ट्र का समस्त इतिहास इससे सम्बद्ध रहा है। हमारे समग्र विचार और आदर्श इस नाम के साथ इतनी घनिष्टता से सम्बन्धित हैं कि इसकी एक सरल परिभाषा करना कठिन होगा। कवियों, पैगम्बरों और अवतारों ने इस नाम की महिमा गायी है। ऋषि-मुनि और सन्तों ने इस राष्ट्र के लिए शास्त्रों एवं दर्शनों की रचना करने हेतु जन्म लिया। वीरों और योद्धाओं ने इसकी प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिये। धर्मनिष्ठा, श्रेष्ठता, उदारता, दर्शन, धार्मिक प्रवृत्ति, योग, धार्मिक सहिष्णुता, प्रज्ञा, भक्ति, वैराग्य, आत्मसाक्षात्कार, सत्य, अहिंसा और शुचिता-ये सब 'हिन्दू' नाम से सम्बद्ध हैं।
-------------------------
१ नवीन शोधों के अनुसार आर्य-प्रजाति के लोग बाहर से नहीं आये थे। वे भारत के मूल निवासी थे।
भारत की आध्यात्मिक भूमि
भारतवर्ष वह पावन भूमि है जिसने असंख्य ऋषियों, मुनियों, योगियों, सन्तों और पैगम्बरों को जन्म दिया है। इसने शंकर, श्री रामानुज जैसे आध्यात्मिक आचार्यों; कबीर, रामदास, तुकाराम, गौरांग महाप्रभु जैसे सन्तों; ज्ञानदेव, दत्तात्रेय, सदाशिवब्रह्मेन्द्र जैसे योगियों और बुद्ध एवं नानक जैसे पैगम्बरों को जन्म दिया। बुद्ध हमारे ही रक्त-मांस हैं।
भारत को गुरु गोविन्दसिंह तथा शिवाजी पर, राजा भोज और विक्रमादित्य पर, शंकर और कबीर पर, वाल्मीकि और कालिदास पर गर्व है। कृष्ण, राम एवं समस्त अवतारों ने भारत में जन्म लिया। कितना पवित्र है भारतवर्ष ! कितना भव्य है भारत ! वृन्दावन और अयोध्या की धरती की धूलि जिस पर कृष्ण और राम ने पावन चरण रखे, अब भी असंख्य लोगों के हृदयों को पवित्र करती है। महात्मा ईसामसीह ने भी अपने जीवन के अज्ञात काल में कश्मीर में रह कर भारतीय योगियों से योग सीखा था। धन्य है भारतभूमि!
भारतवर्ष आध्यात्मिक देश है। भारत ने कभी दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करके उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं किया। सैनिक-विजय कभी उसका आदर्श नहीं रहा। उसकी सदैव यही कामना रही है कि उसके वासी आत्म-स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करें। भारत माता कभी दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं कहती। वह चाहती है कि उसकी सन्तान बाह्य और आन्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करे; दिव्य गुण, नैतिक ऊर्जस्विता एवं आत्म-प्रज्ञा-जनित आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति से सम्पन्न हो। आध्यात्मिक विजय और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने हेतु उसका शस्त्र है-अहिंसा।
भारतवासियों का लक्ष्य है आत्मसाक्षात्कार। वे भौतिक समृद्धि और उन्नति को अधिक महत्त्व नहीं देते। उन्हें चाहिए योग (अथवा परम सत्ता के साथ सम्पर्क)। वे अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर परम साक्षात्कार करने के लिए किसी भी वस्तु का, सर्वस्व का, समस्त सांसारिक उपलब्धियों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति सदा आध्यात्मिक रहती है।
भारत की पावन भूमि में अनेक पवित्र नदियाँ बहती हैं। यहाँ शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंगें समायी हुई हैं। श्वेत बर्फ से आच्छादित पुरातन हिमालय समग्र विश्व के लोगों को आकर्षित करता है। यह भूमि विशेष रूप से ध्यान, चिन्तन और योगाभ्यास के लिए उपयुक्त है। भारतवर्ष योगियों और सन्तों का देश है-यह भारत की एक विशिष्टता है जो दूसरों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि अमरीका, इंग्लैण्ड और विश्व के प्रत्येक भाग से लोग योगाभ्यास के लिए भारत आते हैं।
ऐतिहासिक तथ्य
भारतवर्ष विश्व में सर्वाधिक सहिष्णु देश है। इसका हृदय अति उदार है। अपने स्नेहालिंगन में इसने समस्त राष्ट्रों को समाहित कर लिया है।
पाश्चात्य जातियाँ मूल हिन्दुओं अथवा आर्यों की ही वंशज हैं। वे आर्यों तथा हिन्दू-संस्कृत से अपने पुराने सम्बन्धों को भूल गये होंगे; परन्तु इतिहास इन्हें नहीं भुलायेगा। हिन्दू-संस्कृति की आश्रय भारत माता समुद्र पार रहने वाली अपनी सन्तानों को नहीं भूल सकती। वे उसे सदैव प्रिय हैं।
प्राचीन काल में हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू-सभ्यता अपनी पराकाष्ठा पर थी। ग्रीस तथा रोम के निवासियों ने हिन्दुओं का अनुकरण करके उनके विचारों को ग्रहण कर लिया। किसी भी धर्म में इतने महान् सन्त, महात्मा, योगी, ऋषि, महर्षि, पैगम्बर, आचार्य, परोपकारी, योद्धा, कवि, राजनीतिज्ञ और नरेश नहीं हुए जितने हिन्दू-धर्म में। देश के प्रत्येक प्रान्त ने बुद्धिजीवियों, कवियों और सन्तों को जन्म दिया है। अभी तक भारतवर्ष में ऋषि, दार्शनिक, सन्त और उच्च श्रेणी के बुद्धिमानों की प्रचुरता है। अभी भी यहाँ सन्त-महात्माओं का बाहुल्य है।
हिन्दुओं को युद्ध, कठिनाइयों, विपत्तियों और क्रूरता का सामना करना पड़ा। फिर भी वे जीवित हैं। किसी रहस्यात्मक शक्ति ने उनकी रक्षा की है, किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बचाया है। वही शक्ति सदा उनकी रक्षा करेगी।
हिन्दू-धर्म की उत्तरजीविता के कारण
हिन्दू-धर्म न तो तपश्चर्या है न मायावाद, न बहुदेववाद है और न सर्वेश्वरवाद। यह सब प्रकार के धार्मिक अनुभवों का समन्वय है। यह जीवन का एक सम्पूर्ण दृष्टिकोण है। इसमें हैं व्यापक सहिष्णुता, मानवता की गहराइयाँ और उच्च आध्यात्मिक ध्येय। यह धर्मोन्माद से मुक्त है। इसीलिए यह विश्व के अन्य महान् धर्मों के अनुयायियों के आक्रमणों के पश्चात् भी जीवित है।
कोई भी धर्म इतना उदार और सहिष्णु नहीं जितना हिन्दू-धर्म। हिन्दू-धर्म अपने मूल-तत्त्वों के विषय में अत्यन्त कठोर है; परन्तु बाह्य तथा अतात्त्विक स्वरूपों में पुनर्व्यवस्था के दृष्टिकोण से अत्यन्त उदार है। इसी कारण यह सहस्रों वर्षों से जीवित है।
हिन्दू-धर्म की नींव आध्यात्मिक सत्यों की तलशिला पर पड़ी है। हिन्दू-जीवन की सम्पूर्ण संरचना हिन्दू-ऋषियों और द्रष्टाओं द्वारा प्राप्त शाश्वत सत्यों पर आधारित है। यही कारण है कि यह संरचना अनेक शताब्दियों से जीवित है।
इसका भविष्य
हिन्दू-धर्म की महिमा अनिर्वचनीय है। इसमें वैश्व-धर्म के समस्त लक्षण हैं। इसके सिद्धान्त तथा मत सार्वभौमिक एवं भव्य हैं। इसका दर्शन महान् है। इसकी नीति आत्मा को उन्नत बनाने वाली है। इसके धर्मग्रन्थ अद्भुत हैं। योग-वेदान्त पर आधारित इसकी साधनाएँ अद्वितीय हैं। इस धर्म का भूतकाल अत्यन्त गौरवशाली रहा है। इसका भविष्य और भी अधिक गौरवमय। इसके पास घृणा, मतभेदों और युद्धों से विघटित हुए विश्व के लिए एक सन्देश है-जो ब्रह्माण्डीय प्रेम, सत्य और अहिंसा का सन्देश है, आत्मिक एकता का सन्देश है।
जितना अधिक आप भारत और हिन्दू-धर्म के निकट आयेंगे, उतना ही अधिक आप उसे प्रेम और श्रद्धा देने लगेंगे, और उतना ही अधिक आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जायेंगे; क्योंकि इस निकटता से आपमें जाग्रत होगी योगाभ्यास में रुचि तथा आप आत्मसात् करेंगे हिन्दू-धर्म की आत्मा को।
धन्य है भारत देश! धन्य है हिन्दू धर्म ! धन्य-धन्य हैं वे ऋषि और द्रष्टा जिन्होंने हिन्दू-धर्म की ज्वाला को प्रज्वलित रखा है!
द्वितीय अध्याय
हिन्दू-धर्मग्रन्थ
संस्कृत साहित्य
संस्कृत साहित्य को छह शास्त्रसम्मत और चार ऐहिक शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। शास्त्रसम्मत साहित्य के अन्तर्गत हैं हिन्दुओं के प्रामाणिक धर्मग्रन्थ। प्राचीन संस्कृत साहित्य के परवर्ती विकास काल में ऐहिक साहित्य का सर्जन हुआ है।
धर्मग्रन्थ छह हैं-श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, आगम और दर्शन।
ऐहिक साहित्य के अन्तर्गत चार प्रकार के व्यावहारिक ग्रन्थ हैं-सुभाषित, काव्य, नाटक और अलंकार।
धर्मग्रन्थ
श्रुतियाँ
श्रुतियाँ वेद कहलाती हैं। हिन्दुओं को अपना धर्म वेदों के माध्यम से श्रुतिप्रकाश द्वारा प्राप्त हुआ है। ये सहज ज्ञान द्वारा प्राप्त अनुभूति हैं और इन्हें अपौरुषेय अर्थात् नितान्त परा-मानवीय माना जाता है। इनका कोई विशिष्ट लेखक नहीं है। वेद हिन्दुओं का-नहीं, अखिल विश्व का-महिमाशाली गौरव है।
वेद शब्द की उत्पत्ति विद् धातु से हुई है, जिसका अर्थ है-धर्मग्रन्थ के सन्दर्भ में जानना। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इसका तात्पर्य ज्ञान के ग्रन्थ से हैं। वेद हिन्दुओं के आधारभूत ग्रन्थ हैं। वेद न केवल अन्य पाँच धर्मग्रन्थों वरन् उपर्युक्त चार ऐहिक के भी स्रोत हैं। वेद भारतीय प्रज्ञा की निधि हैं जिन्हें मनुष्य शाश्वतकाल-पर्यन्त विस्मृत नहीं कर सकता।
अनादि तथा अनन्त सत्य की अभिव्यक्ति
वेद भारत के महान् प्राचीन ऋषियों को ईश्वर द्वारा अनुभव करवाये गये शाश्वत सत्य हैं। ऋषि शब्द दृश् धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। ऋषि मन्त्र अर्थात् विचार के द्रष्टा हैं। विचार उनके अपने नहीं थे। ऋषियों ने सत्य को देखा या सुना; इसलिए वेद वे हैं जो श्रवण किये जाते हैं। ऋषियों ने उन्हें लिखा नहीं; ये उनके मस्तिष्क की उपज नहीं हैं। वे उन विचारों के द्रष्टा थे जो पहले से ही प्रचलित थे। उन्होंने मात्र उन विचारों का आध्यात्मिक अन्वेषण किया। वे ही विचार के आध्यात्मिक ज्ञाता थे। वे वेदों के आविष्कारक नहीं हैं।
वेदों में प्राचीन ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभव प्रस्तुत किये गये हैं। ऋषि मात्र अपने अन्तर्जात अनुभवों को लोगों तक पहुँचाने के माध्यम हैं। वेदों के सत्य प्रकटन हैं। विश्व के अन्य सब धर्म यह कहते हैं कि ईश्वर के विशेष दूतों ने उन्हें (धर्मों को) कुछ विशिष्ट लोगों को ही प्रदान किया था, किन्तु वेद अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति के ऋणी नहीं हैं। वे स्वतः प्रमाण हैं; क्योंकि वे शाश्वत हैं, वे ईश्वरीय ज्ञान हैं।
स्रष्टा ब्रह्मा ने ऋषियों अर्थात् द्रष्टाओं को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। ऋषियों ने उस ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया। वैदिक ऋषि दिव्य अनुभूति प्राप्त महान् व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रह्म या सत्य का साक्षात्कार किया था। वे ईश्वर-प्रेरित लेखक थे। उन्होंने धर्म और दर्शन के एक ऐसे सरल, विशाल एवं पूर्ण शास्त्र का विकास किया जिससे समस्त धर्मों के संस्थापकों और गुरुओं ने प्रेरणा प्राप्त की।
वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ हैं। समस्त धर्मों के सत्य वेदों से प्रसूत हैं और अन्ततोगत्वा वेद ही उनके स्रोत हैं। वेद धर्म का मूल स्रोत हैं। वेद ही समस्त धार्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। धर्म का उद्गम दैवी है। प्रारम्भिक काल में यह ईश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए प्रकट किया गया। धर्म का मूर्त रूप वेद हैं।
वेद शाश्वत हैं, अनादि हैं, अनन्त हैं। कोई अज्ञानी पुरुष कह सकता है कि कोई पुस्तक बिना आदि और अन्त के कैसे हो सकती है। वेदों का अभिप्राय किसी पुस्तक से नहीं है। वेद ईश्वर के शब्द हैं। वेद ईश्वर के श्वास से उद्भूत शब्द हैं। वे ईश्वर के शब्द हैं। वेद मनुष्यों के वचन नहीं हैं, वे किसी मानवीय मस्तिष्क की रचना नहीं हैं। वे कभी लिखे नहीं गये, कभी रचे नहीं गये। वे शाश्वत हैं, अव्यक्तिक हैं। वेदों की तिथियाँ निश्चित नहीं की गयी हैं और न कभी की जा सकती हैं। वेद शाश्वत आध्यात्मिक सत्य हैं। वेद दिव्य ज्ञान के मूर्त रूप हैं। पुस्तकें नष्ट हो सकती हैं; परन्तु ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान शाश्वत है, इसी दृष्टि से वेद शाश्वत हैं।
चार वेद और उनके उपविभाग
वेद चार विशाल ग्रन्थों में विभाजित हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है-शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण अथवा तैत्तिरीय अधिक प्राचीन पुस्तक है। शुक्ल अथवा वाजसनेय में देदीप्यमान सूर्य देवता द्वारा याज्ञवल्क्य ऋषि के समक्ष किये गये दिव्य रहस्यों के उद्घाटन हैं।
ऋग्वेद २१ अनुच्छेदों में विभाजित है, यजुर्वेद १०९ में, सामवेद १००० में और अथर्ववेद ५० में। इस प्रकार सम्पूर्ण वेद ११८० अनुच्छेदों में विभाजित है।
प्रत्येक वेद में चार भाग हैं-मन्त्रसंहिता अथवा स्तोत्र, ब्राह्मण अथवा मन्त्रों तथा कर्मकाण्डों की व्याख्या, आरण्यक तथा उपनिषद् । वेदों का चार भागों में विभाजन मानव-जीवन की चार अवस्थाओं (आश्रमों) के अनुकूल है।
मन्त्रसंहिता इहलोक में भौतिक समृद्धि और परलोक में सुख प्राप्ति के लिए वैदिक ईश्वर तथा देवी-देवताओं की प्रशंसा में गाये हुए स्तोत्र हैं। वे विभिन्न प्रकार के देवी-देवताओं को सम्बोधित ऐहिक तथा पारलौकिक विषयक छन्दबद्ध प्रार्थनाएँ, स्तोत्र और मन्त्र हैं। वेदों का मन्त्र-भाग ब्रह्मचारियों के लिए विशेष उपयोगी है।
वेदों के ब्राह्मण-भाग मनुष्यों को यज्ञ आदि यज्ञीय कर्मकाण्ड करने में सहायता करते हैं। इनमें यज्ञ में मन्त्रों का उपयोग करने की गद्यात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। ब्राह्मण-भाग गृहस्थों के लिए उपयोगी है।
आरण्यक वन्य पुस्तकें हैं, जिनमें कर्मकाण्डों की दार्शनिक व्याख्या दी गयी है। आरण्यक वानप्रस्थियों के लिए हैं।
उपनिषद् वेदों के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंश हैं। वेदों का ज्ञान साररूप में उपनिषदों में ही है। उपनिषदों का दर्शन भव्य, गम्भीर, उच्च और मर्मस्पर्शी है। उपनिषद् परमात्मा तथा जीवात्मा का ऐक्य उद्घोषित करते हैं। उनमें अत्यन्त सूक्ष्म एवं गम्भीर आध्यात्मिक सत्यों का उद्घाटन हुआ है। उपनिषद् संन्यासियों के लिए उपयोगी हैं।
समग्र वेद की विषयसामग्री कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड में विभाजित है। कर्मकाण्ड विभिन्न यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों से सम्बन्धित है। उपासनाकाण्ड में ध्यान उपासना के विभिन्न प्रकारों और ज्ञानकाण्ड में निर्गुण ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान का निरूपण किया गया है। मन्त्र तथा ब्राह्मण ग्रन्थ कर्मकाण्ड से सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार आरण्यक ग्रन्थ उपासनाकाण्ड एवं उपनिषद् ज्ञानकाण्ड से सम्बन्धित हैं।
मन्त्रसंहिता
ऋग्वेदसंहिता हिन्दुओं का प्रधान, प्राचीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। यह भारत की महान् बाइबिल है। इसकी शैली-भाषा एवं श्वर-शैली अत्यन्त सुन्दर तथा रहस्यमय हैं। इसके अमर मन्त्र अस्तित्व के महान् सत्यों के प्रतीक हैं। यह सम्भवतः विश्व के समस्त धर्मग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका याजक 'होतृ' कहलाता है।
यजुर्वेदसंहिता का अधिकांश भाग गद्य में है। यजुर्वेद के याजक (अध्वर्यु) यज्ञीय कर्मकाण्डों की व्याख्या करने के लिए इसे उपयोग में लाते हैं। यह ऋग्वेद के मन्त्रों का पूरक है।
सामवेदसंहिता का अधिकांश ऋग्वेदसंहिता ही है। यह सामवेद के याजक (उद्गातृ) के द्वारा यज्ञ में गाये जाने के लिए है।
अथर्ववेदसंहिता अथर्ववेद के याजक ब्रह्मा द्वारा उपयोग में लायी जाती है ताकि वह यज्ञ के अन्य तीन याजकों द्वारा संयोगवश किये जाने वाले अशुद्ध उच्चारणों और गलत ढंग से किये जाने वाले कर्मकाण्डों को शुद्ध कर सके।
ब्राह्मण तथा आरण्यक
ऋग्वेद के अन्तर्गत दो ब्राह्मण-ग्रन्थ हैं- ऐतरेय और सांख्यायन। मैक्समूलर के अनुसार, "ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ है। ब्राह्मण ग्रन्थ के पावन स्तोत्र अखिल विश्व के साहित्य में अनुपम हैं और उनका संरक्षण वस्तुतः अद्भुत है।" (History of Ancient Literature)
शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्धित है, तैत्तिरीय और मैत्रायण-ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से। ताण्ड्य अथवा पंचविंश, षड्विंश, छान्दोग्य, अद्भुत, आर्षेय और उपनिषद् ब्राह्मण सामवेद से सम्बन्धित हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण 'गोपथ' कहलाता है। प्रत्येक ब्राह्मण का एक आरण्यक है।
उपनिषद्
उपनिषद् वेदों के उपसंहार-अंश अथवा अन्तिम भाग हैं। उन पर आधारित शिक्षा वेदान्त कहलाती है। उपनिषद् वेदों का लक्ष्य और सारांश हैं। वे हिन्दू-धर्म की आधारशिला ही हैं।
प्रत्येक वेद के उतने ही उपनिषद् हैं जितनी उसकी शाखाएँ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की क्रमशः २१, १०९, १००० तथा ५० शाखाएँ हैं।
भारतवर्ष के विभिन्न मतों (यथा-अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, भेदाभेदवाद आदि) के समर्थक दार्शनिकों ने उपनिषदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को स्वीकार किया है। उन्होंने इन ग्रन्थों की व्याख्याएँ तो की हैं; परन्तु प्रामाणिकता इन्हीं की मानी है। उन्होंने अपनी-अपनी दर्शन-प्रणालियों को उपनिषदों के आधार पर ही विकसित किया है।
उपनिषदों के द्रष्टाओं की पाश्चात्य विद्वानों ने भी प्रशंसा की है। उस समय जब कि पाश्चात्य लोग इतने पिछड़े हुए थे कि छाल के कपड़े और घोर अज्ञानता में डूबे हुए थे, उपनिषदों के द्रष्टा शाश्वत परमानन्द में निमग्न रहते थे तथा उनकी संस्कृति और सभ्यता सर्वोच्चता के शिखर पर थी।
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपनिषद् हैं-ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकी, श्वेताश्वतर तथा मैत्रायणि। ये सब परम अधिकृत ग्रन्थ हैं।
वेदों के मूलभूत सत्य आप सबके समक्ष उद्घाटित हो सकें! वेदों की माता गायत्री आपको ज्ञान-रूपी दूध-उपनिषदों की प्राचीन प्रज्ञा प्रदान करे!
उपवेद
चारों वेदों के पूरक के रूप में उपवेदों की संख्या चार है। ये हैं- आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थशास्त्र। क्रमशः इनका अर्थ इस प्रकार है-आयुर्विज्ञान, युद्ध-विज्ञान, संगीत-विज्ञान एवं राजशासन (polity) का विज्ञान ।
वेदांग
वेदों के छह व्याख्यात्मक अंग हैं-पाणिनि की शिक्षा और व्याकरण, पिंगलाचार्य का छन्द, यास्क का निरुक्त, गर्ग का ज्योतिष और विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित कल्प-श्रौत, गृह्य, धर्म एवं शुल्ब।
शिक्षा स्वर-विज्ञान का ज्ञान है। यह वेदांग उच्चारण और स्वराघात से सम्बन्धित है। वेदों की सामग्री विभिन्न पाठों में विभाजित है। पद-पाठ में प्रत्येक शब्द को एक अलग रूप दे कर समझाया गया है। क्रम-पाठ में शब्दों को जोड़ों (pairs) में व्यवस्थित किया गया है।
व्याकरण से तात्पर्य संस्कृत व्याकरण से है। पाणिनि के ग्रन्थ अति-प्रसिद्ध हैं। व्याकरण के ज्ञान के अभाव में आप वेदों को नहीं समझ सकते।
छन्द में पिंगल के छन्दों (metre) की व्याख्या है।
निरुक्त भाषा-शास्त्र है।
ज्योतिष में खगोलविज्ञान और फलित ज्योतिष की व्याख्या है। इसमें नक्षत्र आदि की गतियों और मानव पर उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है।
कल्प कर्मकाण्ड की प्रणाली है। यज्ञीय कर्मकाण्ड का निरूपण करने वाले श्रौत-सूत्र कल्प के अन्तर्गत आते हैं। शुल्बसूत्र में यज्ञ-क्षेत्र की नापों का वर्णन है। ये सूत्र भी कल्प के अन्तर्गत हैं। गृहस्थ जीवन पर प्रकाश डालने वाले गृह्य-सूत्र और नैतिकता, रीति-रिवाजों तथा विधि-विधानों की व्याख्या करने वाले धर्म-सूत्र भी कल्प के अन्तर्गत हैं।
प्रतिशाख्य, पदपाठ, क्रमपाठ, उपलेख, अनुक्रमणि, दैवत-संहिताएँ, परिशिष्ट, प्रयोग, पद्धतियाँ, कारिकाएँ, खिल और व्यूह कल्प-सूत्रों में वर्णित कर्मकाण्डों को और अधिक सविस्तार प्रतिपादित करते हैं।
कल्प-सूत्रों के अन्तर्गत अश्वलायन, शाख्यायन और साम्भाव्य ऋग्वेद के हैं। मशक, लाट्यायन, द्रह्यायन, गोभिल और खादिरा सामवेद के हैं। कात्यायन और पारस्कर शुल्क यजुर्वेद के हैं। आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, मानव, वैखानस और काठक कृष्ण यजुर्वेद के हैं तथा वैतान और कौशिक अथर्ववेद के हैं।
स्मृतियाँ
श्रुतियों के बाद स्मृतियों का महत्त्व है। ये हिन्दुओं के सनातन वर्णाश्रम-धर्म से सम्बन्धित पावन प्राचीन नियमसंहिताएँ हैं। वेदों में दिये हुए कर्मकाण्ड सम्बन्धी आदेशों (विधियों) की ये पूरक हैं और उनकी व्याख्या करती हैं। स्मृति अथवा धर्मशास्त्र की आधारशिला श्रुति है। स्मृति-ग्रन्थ वेदों के उपदेशों पर आधारित हैं। प्रामाणिकता में स्मृति का स्थान श्रुति के बाद दूसरा है। यह धर्म का निरूपण और विकास करती है। यह हिन्दू राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का नियमन करने वाले नियमों और कानूनों का निरूपण करती है।
प्रत्यक्ष रूप से स्मृति कहलाने वाले ग्रन्थ धर्मशास्त्र (संहिताओं की पुस्तक) हैं। व्यापक रूप में स्मृति के अन्तर्गत वेदों के अतिरिक्त समस्त हिन्दू-शास्त्र आ जाते हैं।
समय-समय पर हिन्दू-समाज का नियमन करने वाले नियम स्मृतियों में निहित हैं। उनमें व्यक्तियों तथा समुदायों के लिए दैनिक आचरण में मार्गदर्शन देने के लिए और उनके रीति-रिवाजों को व्यवस्थित करने के निश्चित नियम दिये हुए हैं। स्मृतियों में प्रत्येक श्रेणी के मनुष्यों को परिस्थितियों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करने से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।
इन स्मृतियों से हिन्दू अपना जीवन यापन करना सीखता है। वर्णाश्रम के कर्तव्यों तथा समस्त धर्मानुष्ठानों का विवेचन उन ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से किया गया है। स्मृतियों में मनुष्य के जन्म और आश्रम के अनुसार कुछ कर्मों का निर्धारण किया गया है और कुछ का निषेध। स्मृतियों का ध्येय है मानव-हृदय को परिशुद्ध करके उसे धीरे-धीरे अमरत्व के परम पद पर ले जाना तथा उसे पूर्ण एवं मुक्त बनाना।
ये स्मृतियाँ समय-समय पर बदलती रही हैं। स्मृतियों के आदेश तथा निषेध विशेष सामाजिक प्रतिवेश से सम्बन्धित होते हैं। जैसे जैसे हिन्दू-समाज के प्रतिवेश एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होते गये, वैसे-वैसे विभिन्न काल के ऋषियों द्वारा नयी-नयी स्मृतियों का संकलन होता रहा है।
प्रसिद्ध हिन्दू-विधिकर्ता
समय-समय पर कोई-न-कोई महान् विधिकर्ता जन्म लेता रहा है। वह प्रचलित नियमों को विधिबद्ध (codify) करता है तथा उन नियमों को हटा देता है जो पुराने पड़ गये हैं। वह उनमें कुछ परिवर्तन करके, घटा-बढ़ा कर उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप बना देता है, ताकि वेद की शिक्षा के अनुकूल लोग जीवन व्यतीत कर सकें। इन विधिकर्ताओं में मनु, याज्ञवल्क्य और पाराशर सुप्रसिद्ध हैं। हिन्दू-समाज इन्हीं तीन महान् विधिकर्ताओं द्वारा रचित नियमों पर आधारित है और उनके द्वारा संचालित होता है। विशेष रूप से उल्लेखनीय स्मृतियाँ इन्हीं तीन विधिकर्ताओं द्वारा रचित हैं, यथा- (१) मनुस्मृति अर्थात् मानव-धर्म-शास्त्र, (२) याज्ञवल्क्यस्मृति और (३) पाराशरस्मृति। मनु एक महानतम तथा प्राचीनतम विधिकर्ता हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति मनुस्मृति की ही है और महत्त्व में उससे द्वितीय स्थान पर है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति वर्तमान समय में भारत-भर में प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं। हिन्दू-विधि से सम्बन्धित विषयों में मुख्यतः याज्ञवल्क्यस्मृति का ही ध्यान रखा जाता है। भारत सरकार ने भी प्राचीन कानूनों में से कुछ को मान्यता दे दी है।
मुख्य स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र अठारह हैं। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्मृतियाँ मनु, याज्ञवल्क्य और पाराशर द्वारा रचित हैं। शेष पन्दरह स्मृतियाँ हैं-विष्णु, दक्ष, संवर्त, व्यास, हारीत, शततप, वसिष्ठ, यम, आपस्तम्ब, गौतम, देवल, शंख-लिखित, उशन, अत्रि और शौनक।
मनु के नियम सत्ययुग के लिए हैं। याज्ञवल्क्य के त्रेतायुग के लिए, शंख और लिखित के नियम द्वापर के लिए एवं पाराशर के नियम कलियुग के लिए हैं।
जो नियम नितान्त सामाजिक परिस्थिति, समय और वातावरण पर आधारित हैं, उन्हें समाज, समय और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ परिवर्तित होते रहना चाहिए, तभी हिन्दू-समाज की उन्नति सुनिश्चित हो सकती है।
नवीन नियमावली की आवश्यकता
वर्तमान समय में मनु के द्वारा रचे हुए कुछ नियमों का अक्षरशः पालन करना सम्भव नहीं है। उनके भाव को ही ग्रहण किया जा सकता है, शब्दों को नहीं। समाज प्रगति कर रहा है। जब समाज विकसित होता है, तब वह उन विधि-नियमों से आगे बढ़ जाता है जो भूतकाल में कभी समाज के विकास में योगदान दे रहे थे। कई नवीन विचार जिनके विषय में विधिकर्ताओं ने सोचा भी नहीं था, अब उत्पन्न हो गये हैं। जो नियम पुराने पड़ गये हैं, उनका पालन करने के लिए लोगों से आग्रह करना व्यर्थ है।
हमारा वर्तमान समाज बहुत परिवर्तित हो गया है। अब इस युग की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नयी स्मृति की आवश्यकता है। कोई अन्य मनीषी आज के हिन्दू-समाज के समक्ष नयी नियमावली प्रस्तुत करेगा, इसके लिए उपयुक्त समय अब आ गया है। वर्तमान समय का स्वागत है।
अन्तःस्वर
तप, जप, कीर्तन, ध्यान तथा गुरु-सेवा के द्वारा जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, जिसका अन्तःकरण बिलकुल पवित्र है, उसे धर्म, कर्तव्य अथवा नैतिक कमर्मों में उसका अन्तःस्वर ही मार्ग-निर्देशन प्रदान करता है। सत्त्व-भाव से परिपूर्ण शद्ध हृदय का अन्तःस्वर वास्तव में उस अन्तर्यामी भगवान् की ही पुकार है जो हमारा आन्तरिक शासक है। यह स्वर स्मृति के विधि-विधानों से भी बढ़ कर है। यह स्मृतियों की स्मृति है। अपने हृदय को पवित्र बनायें और उस अन्तःस्वर को सुनने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करें। इस स्वर का श्रवण करने के लिए अपने कानों को समाचरित करें।
श्रुति और स्मृति
श्रुति और स्मृति हिन्दू-धर्म के दो प्रामाणिक स्रोत हैं। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है- 'जो सुना जाता है' और स्मृति का अर्थ है- 'जो स्मरण किया जाता है'। श्रुति प्रकटन है और स्मृति परम्परा। उपनिषद् श्रुति हैं, गीता स्मृति है।
श्रुति साक्षात् अनुभव है। महान् ऋषियों ने धर्म के शाश्वत सत्यों को श्रवण करके उनका आलेख आने वाली पीढ़ियों लाभ लिए छोड़ दिया। इन आलेखों से वेद बने। इस प्रकार श्रुति मूल-प्रमाण है। स्मृति अनुभव का अनुस्मरण है। इसीलिए स्मृति का स्थान प्रमाण के रूप में श्रुति के बाद है। स्मृतियाँ अथवा धर्मशास्त्र भी सन्तों द्वारा लिखित ग्रन्थ हैं; किन्तु वे अन्त्य-प्रमाण नहीं हैं। यदि स्मृति में श्रुति का खण्डन करने वाली कोई बात होगी, तो स्मृति अमान्य हो जायेगी।
इतिहास-ग्रन्थ
मैत्री-प्रबन्ध और आदेशात्मक-प्रबन्ध
इस शीर्षक के अन्तर्गत चार ग्रन्थ हैं- वाल्मीकि रामायण, योगवासिष्ठ, महाभारत और हरिवंश। वेदों में जो है, वह इनमें भी है; परन्तु अधिक सरल रूप में है। ये सुद्धत-संहिताएँ अर्थात् मैत्री-प्रबन्ध कहलाते हैं तथा वेद प्रभु संहिताएँ अर्थात् आदेशात्मक-संहिता जो अत्यन्त प्रामाणिक हैं। इन रचनाओं में ऐतिहासिक वर्णनों, कहानियों और कथोपकथन के रूप में सार्वभौमिक सत्यों की व्याख्या है। ये अत्यन्त मनोरंजक ग्रन्थ हैं जो बालकों से ले कर बुद्धजीवी विद्वानों तक सभी को रुचिकर लगते हैं।
इतिहास-ग्रन्थों में अत्यन्त रोचक और महत्त्वपूर्ण कथाएँ दी हुई हैं जिनके माध्यम से हिन्दू-धर्म के समस्त मूलभूत उपदेश पाठक के मन में स्थायी रूप से अंकित हो जाते हैं।
स्मृति-ग्रन्थों के नियमों और वेदों के सिद्धान्तों की छाप हिन्दू-पाठकों के मन पर उनके राष्ट्रीय वीरों के चमत्कारिक तथा श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से पड़ती है। इन उत्कृष्ट कथाओं से हमें हिन्दू-धर्म का स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है।
सामान्य व्यक्ति के लिए उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों का गूढ़ दर्शन बोधगम्य नहीं है; इसलिए वाल्मीकि और व्यास ने जनसाधारण के लिए इतिहास लिखे जिनमें वेदों का गूढ़ दर्शन सर्वसाधारण के लिए उदाहरणों और आख्यानों के माध्यम से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
दो सुप्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्थ रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं। वे हिन्दुओं के अति-प्रसिद्ध और उपयोगी शास्त्र हैं। रामायण ऋषि वाल्मीकि द्वारा और महाभारत व्यास जी द्वारा विरचित हैं।
रामायण
रामायण में आदर्श पुरुष राम की कथा वर्णित है। यह इक्ष्वाकु के वंशज सूर्यवंशी राजाओं के परिवार का इतिहास है जिसमें भगवान् विष्णु के अवतार रामचन्द्र और उनके तीन भाई जन्मे थे। रामायण के राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और श्री हनुमान् जैसे आदर्श चरित्र हमारे मन पर हिन्दू-धर्म की स्पष्ट छाप छोड़ते हैं। राम और उनके भाइयों के जन्म, उनकी शिक्षा और विवाह, श्रीराम वनवास, सीता का हरण और उनकी प्रतिप्राप्ति, रावण-वध और श्रीराम-राज्य आदि के विवरण रामायण में विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किये गये हैं। मनुष्य को अपने से बड़ों, समवयस्कों और छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए, मनुष्य को इस संसार में कैसे जीवन-यापन करना चाहिए, वह किस प्रकार मोक्ष, स्वतन्त्रता और पूर्णता प्राप्त कर सकता है-यह सब इस सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ से सीखा जा सकता है। रामायण से भारतीय जीवन की स्पष्ट झाँकी देखने को मिलती है। आज भी हमारे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आदर्शों के स्रोत रामायण और महाभारत के ये उच्च चरित्र ही हैं। इन ग्रन्थों के महान् राष्ट्रीय नायक आज भी प्रकाश स्तम्भ की तरह समस्त विश्व की जनता का पथ-प्रदर्शन करते और प्रेरणा प्रदान करते हैं। राम, भरत और लक्ष्मण के जीवन भ्रातृ-स्नेह और पारस्परिक सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान् एक असाधारण कर्मयोगी के रूप में उभर कर आते हैं। सीता का जीवन पतिव्रतधर्म, पवित्रता और माधुर्य का अनुपम उदाहरण है। श्री वाल्मीकि ने रामायण (जो आदि-काव्य है) में चौबीस हजार श्लोक लिखे हैं।
महाभारत
महाभारत कौरवों और पाण्डवों का इतिहास है। इसमें चन्द्रवंशी कौरवों और पाण्डवों के बीच कुरुक्षेत्र में होने वाले महायुद्ध का वर्णन है। कौरव और पाण्डव परस्पर चचेरे भाई थे। महाभारत हिन्दू-धर्म का विश्वकोश है। इसे पाँचवाँ वेद कहना उपयुक्त ही है। धर्म, दर्शन, रहस्यवाद और राज्यतन्त्र के अन्तर्गत कोई भी विषय ऐसे नहीं हैं जिनका वर्णन इस महाकाव्य में न हुआ हो। इसमें अत्युच्च नैतिक शिक्षाएँ, कई सुन्दर कथाएँ, उपाख्यान, भाषण, धर्मोपदेश तथा दृष्टान्त हैं। इन्हीं के माध्यम से नीति और तत्त्वमीमांसा के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। भगवान् कृष्ण की कृपा से पाण्डवों ने विजय प्राप्त की। श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने इस महाकाव्य की रचना की। इसमें एक लाख श्लोक हैं।
भगवद्गीता
महाभारत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग भगवद्गीता है, महाभारत के युद्ध के प्रारम्भ होने से पूर्व रण-क्षेत्र में भगवान् कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला यह अद्भुत वार्तालाप है। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथि बने, उन्होंने अर्जुन को हिन्दू-धर्म के मूलभूत सिद्धान्त समझाये। जिस प्रकार उपनिषद् वेदों का सार है, उसी प्रकार गीता उपनिषदों का सार है। उपनिषद् गौ के समान है, कृष्ण जी ग्वाले हैं, अर्जुन बछड़ा और गीता दूध है। जो गीता-रूपी दुग्ध का पान करते हैं, वे बुद्धिमान् व्यक्ति हैं।
गीता हिन्दू-साहित्य का अमूल्य रत्न है। यह सार्वभौमिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती है। गीता समन्वययोग की शिक्षा देती है। विश्व के धार्मिक साहित्य में इसका उच्च स्थान है।
युद्ध-क्षेत्र में अपने सामने अपने प्रिय सम्बन्धियों और गुरु जनों को खड़े देख कर अर्जुन मूर्च्छित हो गया और उसने उनसे युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब भगवान् कृष्ण ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया और उसे विश्वास दिलाया कि फल की चिन्ता किये बिना युद्ध करना उसका कर्तव्य है। तत्पश्चात् अर्जुन के मोह तथा संशय दूर हो गये। वह कौरवों ये युद्ध करके विजयी हुआ।
प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान
महाभारत में धर्म-विषय पर भीष्म की वह अमर चर्चा भी है जो उन्होंने बाणों की शय्या पर लेटे-लेटे युधिष्ठिर से की थी। समग्र महाभारत इतिहास, नीति और धर्म का एक अद्वितीय विश्वकोश बन गया है।
रामायण और महाभारत में हमें प्राचीन भारत, उसके निवासियों, प्रथाओं, रहन-सहन के ढंग, कला, सभ्यता और संस्कृति तथा उसके उद्योगों का स्पष्ट विवरण मिलता है। इन दो ग्रन्थों को पढ़ने से आपको विदित होगा कि कभी भारत कितना महान् था। आपको उसे पुनः महान् बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। अन्य किसी देश में इतने महापुरुष, महान् गुरु, महान् योगी, महान् द्रष्टा, महर्षि, महान् पैगम्बर, महान् आचार्य, महान् नरेश, महान् नायक, महान् राजनेता, महान् देशभक्त और महान् परोपकारी व्यक्ति नहीं हुए जितने भारत में हुए। जितना अधिक आप भारत और हिन्दू-धर्म के बारे में जानेंगे, उतना ही अधिक उसका सम्मान और प्रेम करेंगे और परमात्मा को इस बात का धन्यवाद देंगे कि उसने आपको भारत में हिन्दू बना कर जन्म दिया। धन्य है भारतवर्ष ! धन्य है हिन्दू धर्म ! धन्य है उपनिषदों के द्रष्टा ! धन्य है दिव्य गीतों के रचयिता कृष्ण!
पुराण
पुराण इतिहास की ही श्रेणी के हैं। उनके पाँच लक्षण हैं- (१) सर्ग तथा सृष्टि-विज्ञान; (२) प्रतिसर्ग अर्थात् सृष्टि का विस्तार, लय तथा पुनःसृष्टि आदि; (३) सृष्टि आदि की वंशावली; (४) मन्वन्तर अर्थात् किस-किस मनु का समय कब-कब रहा और उस काल में कौन-कौन-सी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई थीं; और (५) वंशानुचरित अर्थात् राजाओं की वंशावली। समस्त पुराण सुहत्संहिताओं के अन्तर्गत हैं।
युगों-युगों से पुराणों के संकलनकर्ता व्यास हैं और इस युग के लिए वह पराशर के पुत्र कृष्णद्वैपायन हैं।
वेदों के धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए पुराण लिखे गये थे। उनमें वेदों का सार निहित है। पुराणों का लक्ष्य है जन-साधारण के मन पर वेदों की शिक्षा का प्रभाव अंकित करके ठोस उदाहरणों, पौराणिक कथाओं, कहानियों, आख्यानों, सन्तों, राजाओं और महापुरुषों की जीवनियों एवं महान् ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन के माध्यम से उनमें भगवद्भक्ति उत्पन्न करना। धर्म के शाश्वत सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने हेतु सन्तों ने इन माध्यमों का ही उपयोग किया। पुराण विद्वानों के लिए नहीं, सामान्य व्यक्तियों के लिए थे जो उच्च दर्शन नहीं समझ सकते थे तथा जिनमें वेदों का अध्ययन करने की क्षमता भी नहीं थी।
दर्शन का अध्ययन बहुत ही कठिन है। यह केवल थोड़े से विद्वानों के लिए है। पुराण साधारण बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए हैं। पुराणों के माध्यम से धर्म अत्यन्त सरल और रोचक ढंग से सिखाया गया है। आज भी पुराण लोकप्रिय हैं। पुराणों में अति-प्राचीनकाल का इतिहास वर्णित है। उनमें जगत् के उन क्षेत्रों का भी वर्णन है जिन्हें साधारण भौतिक दृष्टि नहीं देख पाती। वे पढ़ने में बड़े मनोरंजक हैं और उनसे सब प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। बच्चे अपनी दादियों से इनकी कहानियों को सुनते हैं। पण्डित और पुरोहित मन्दिरों में, नदियों के तट पर एवं अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों में पुराणों की कथाएँ कहते हैं, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग बड़ी रुचि से सुनते हैं।
अठारह पुराण
अठारह मुख्य पुराण हैं और इतनी ही संख्या में उप-पुराण भी हैं। मुख्य पुराण हैं-विष्णुपुराण, नारदीयपुराण, श्रीमद्भागवतपुराण, गरुड़ (सुपर्ण)-पुराण, पद्मपुराण, वाराहपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, मार्कण्डेयपुराण, भविष्यपुराण, वामनपुराण, मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण, लिंगपुराण, शिवपुराण, स्कन्दपुराण और अग्निपुराण। इनमें छह सात्त्विक पुराण हैं जो विष्णु का गुणगान करते हैं, छह राजसिक हैं जो ब्रह्म की महिमा का वर्णन करते हैं तथा शेष छह तामसिक हैं। जो शिवजी की स्तुति करते हैं।
प्रारम्भिक साधक शिवपुराण या विष्णुपुराण का अध्ययन करके भ्रमित हो जाते है। शिवपुराण में शिवजी की बहुत प्रशंसा की गयी है और भगवान् विष्णु को निम्न स्थान प्रदान किया गया है। विष्णुपुराण में भगवान् हरि की स्तुति की गयी है और भगवान् शिव को गौण स्थान दिया गया है। कभी भगवान् शिव की महिमा कम कर दी है। भक्तों में अपने-अपने इष्टदेवों के प्रति श्रद्धा-भाव विकसित करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया गया है। भगवान् शिव और विष्णु एक हैं।
पुराणों में भागवत और विष्णुपुराण सर्वश्रेष्ठ हैं। भागवत सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके पश्चात् विष्णुपुराण का स्थान है। मार्कण्डेयपुराण का एक अंश चण्डी अथवा देवी-माहात्म्य नाम से प्रसिद्ध है। भगवान् के मातृ-स्वरूप की उपासना ही इस अंश की विषय-सामग्री है। पवित्र पर्वो तथा नवरात्र के अवसर पर चण्डी का पाठ किया जाता है।
श्रीमद्भागवतपुराण और दशावतार
भागवतपुराण भगवान् विष्णु के विभिन्न अवतारों की ऐतिहासिक गाथा है। विष्णु के दश अवतार हुए हैं। प्रत्येक अवतार का उद्देश्य विश्व को किसी महान् संकट से मुक्त करना तथा दुष्टों का संहार करके सज्जनों की रक्षा करना रहा है। ये दश अवतार हैं-मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, श्रीकृष्ण, बुद्ध और कल्कि (सफेद घोड़े पर सवार बीर जो कलियुग के अन्त में जन्म लेगा)।
मत्स्य अवतार का उद्देश्य था जल प्रलय से वैवस्वत मनु को बचाना। कूर्म अवतार का उद्देश्य था प्रलय में खोयी हुई अमूल्य वस्तुओं को संसार को पुनः प्राप्त कराना। जब देव और असुरों ने क्षीर सागर का मन्थन किया, तो कछुए ने रई रखने के लिए अपनी पीठ प्रस्तुत कर दी थी। वामन अवतार का लक्ष्य था धरती की
जल से रक्षा करना जिसे हिरण्याक्ष नामक राक्षस पाताल में घसीट ले गया था। नृसिंह अवतार का लक्ष्य था प्रह्लाद के पिता राक्षस हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से विश्व की रक्षा करना। वामन अवतार का लक्ष्य था राजा बलि की तपस्या और भक्ति से श्रीहीन हुई देवताओं की शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करके उसे देवताओं को लौटाना। परशुराम अवतार का लक्ष्य था क्षत्रिय राजाओं के दबाव से देश को मुक्त करना। परशुराम ने २१ बार क्षत्रिय प्रजाति का संहार किया। श्रीराम के अवतार का लक्ष्य दुष्ट रावण का संहार करना था। श्रीकृष्ण-अवतार का लक्ष्य था कंस और अन्य दानवों को मारना एवं गीता का अनुपम सन्देश दे कर भक्तिमत का प्रचार करना। बुद्धावतार का ध्येय था पशुबलि का अन्त करना और धर्मनिष्ठा का प्रचार-प्रसार करना। कल्कि अवतार का लक्ष्य है दुष्टता का नाश और सद्गुणों की पुनर्स्थापना।
तमिल पुराण
भगवान् शिव ने चार कुमारों को ज्ञान देने के लिए दक्षिणामूर्ति के रूप में अवतार लिया। उन्होंने सम्बन्धार, माणिक्कवासगर और पट्टिनाधर को दीक्षा देने के लिए मानव-रूप धारण किया था। वह अपने भक्तों की सहायता करने और उनके कष्ट हरण करने के लिए साक्षात् मानव-रूप में प्रकट हुए। भगवान् शिव की दिव्य लीलाएँ तमिल पुराणों-यथा शिवपुराण, पेरियपुराणम्, शिवपराक्रमम् तथा तिरुविलयडल- में वर्णित हैं।
उप-पुराण
उप-पुराण संख्या में अठारह हैं-सनत्कुमार, नृसिंह, बृहन्नारदीय, शिवरहस्य, दुर्वासा, कपिल, मानव, भार्गव, वारुण, कालिका, साम्ब, नन्दी, सूर्य, पाराशर, वसिष्ठ, देवी-भागवत, गणेश और हंस।
पुराणों की उपयोगिता
पुराणों का अध्ययन, धर्मग्रन्थों के पावन पाठ का श्रवण और भगवान् की लोकातीत लीलाओं का बखान भक्तों की साधना के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। इनसे भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रवण नवधा-भक्ति का एक अंग है। पुराणों की कथाएँ श्रोताओं के हृदय में प्रेमा-भक्ति का संचार करती हैं। इससे जीव को अमरता प्राप्त होती है।
वेदों की भाषा अप्रचलित है और वेदान्त तथा उपनिषदों का दर्शन अत्यन्त कठिनाई से बोधगम्य हो पाता है। इस दृष्टि से पुराणों का विशेष महत्त्व है; क्योंकि उनमें दार्शनिक सत्यों और अमूल्य उपदेशों को सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया। इनसे जीवन के रहस्यों और परमानन्द प्राप्त करने के उपायों को समझने में सहायता मिलती है। इनके उपदेशों को ग्रहण करें और आज से ही धर्मनिष्ठा और आध्यात्मिक साधना का नया जीवन आरम्भ कर दें।
आगम
प्रचलित धर्मग्रन्थों का एक अन्य वर्ग आगम हैं। आगम ईश्वरपरक ग्रन्थ और देवोपासना की व्यावहारिक नियम पुस्तकें हैं। आगमों में तन्त्र, मन्त्र और यन्त्र सम्मिलित हैं। ये मन्दिरों आदि में की जाने वाली ईश्वर की बाह्य साकार उपासना का वर्णन करने वाले ग्रन्थ हैं। समस्त आगमों में ज्ञान, योग (चित्त की एकाग्रता), क्रिया (दीक्षणीय कर्म-काण्ड) और चर्य्या (बाह्य उपासना) का वर्णन है। इनमें सत्तामीमांसा, ब्रह्माण्डविज्ञान, मुक्ति, ध्यान, मन्त्र, दर्शन, गुह्य मण्डल (diagrams), तन्त्र-मन्त्र, मन्दिर-निर्माण, मूर्ति-निर्माण, घरेलू कार्यकलाप, सामाजिक नियम, सार्वजनिक त्यौहारों आदि का भी वर्णन है।
आगम तीन भागों में विभाजित हैं-वैष्णव, शैव और शाक्त। हिन्दुत्व के तीन मुख्य मत है-वैष्णव, शैव और शाक्त। इनके धर्म-सिद्धान्त सम्बन्धित आगमों पर निर्धारित हैं। वैष्णव अथवा पांचरात्र-आगम भगवान् का विष्णु के रूप में गुणगान करते हैं। शैव-आगम शिव के रूप में भगवान् की महिमा का वर्णन करते हैं। दक्षिण भारत, विशेषकर तिरुनेलवेली और मदुरै जनपदों में प्रचलित शैव-सिद्धान्त नामक महत्त्वपूर्ण दर्शन शैव-आगम पर ही आधारित है। शाक्त-आगम अथवा तन्त्र देवी के विभिन्न नामों के अन्तर्गत विश्वजननी के रूप में ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं।
आगमों की प्रामाणिकता का स्रोत वेद नहीं हैं; परन्तु ये उनके विरोधी भी नहीं हैं। भाव तथा लक्षण में वे सब वैदिक हैं-यही कारण है कि वे प्रामाणिक माने जाते हैं।
वैष्णव-आगम
वैष्णव-आगम चार प्रकार के हैं- वैखानस, पांचरात्र, प्रतिष्ठासार और विज्ञानललित। ब्राह्म, शैव, कौमार, वासिष्ठ, कपिल, गौतमीय और नारदीय-ये पांचरात्र के सात विभाग हैं। महाभारत के शान्ति-पर्व का नारदीय-सर्ग पांचरात्र-सम्बन्धी ज्ञान का सबसे पुराना स्रोत है।
भगवान् विष्णु पांचरात्र-आगमों में परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत हैं। वैष्णव-भक्त पांचरात्र-आगम को सर्वाधिक प्रामाणिक मानते हैं। उनका विश्वास है कि ये आगम स्वयं भगवान् विष्णु द्वारा प्रकटित किये गये। नारद-पांचरात्र में लिखा है-"ब्रह्म से ले कर तृण तक प्रत्येक वस्तु भगवान् कृष्ण है।" यह उपनिषदों के कथन-'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' के सदृश है।
वैष्णव-ग्रन्थों की संख्या २१५ है। इनमें ईश्वर, अहिर्बुध्न्य, पौष्कर, परम, सात्त्वत, बृहद् ब्रह्म और ज्ञानामृतसार संहिताएँ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
शैव-आगम
शैव लोग अट्ठाईस आगमों को मान्यता देते हैं जिनमें मुख्य आगमन 'कामिक' है। कश्मीर शैव-मत (जिसे प्रत्यभिज्ञ-प्रणाली भी कहते हैं) का आधार भी आगम ही हैं। प्रत्यभिज्ञ-प्रणाली के बाद की रचनाओं में अद्वैत की ओर स्पष्ट झुकाव दृष्टिगत होता है। दक्षिण शैव-सिद्धान्त और कश्मीर शैव मत वेदों के अतिरिक्त इन आगमों को भी अपने प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं। प्रत्येक आगम के अन्तर्गत उप-आगम भी हैं। इनमें से केवल बीस के आंशिक अपूर्ण मूल-पाठ उपलब्ध हैं। शैव-आगमों में भगवान् शिव प्रमुख देवता हैं। कलियुग के लिए वह उपयुक्त देव हैं-सभी जाति के स्त्री और पुरुष उनकी उपासना कर सकते हैं।
शाक्त-आगम
धर्मग्रन्थों का एक वर्ग तन्त्र कहलाता है। ये ग्रन्थ शाक्तमत से सम्बन्ध रखते हैं। ये जगज्जननी के रूप में शक्ति-महिमा का वर्णन करते हैं। इनमें भगवान् के शक्ति-रूप का वर्णन है और दिव्य जननी की विभिन्न प्रकार की आनुष्ठानिक उपासना-विधियाँ निर्धारित की गयी हैं। आगमों की संख्या ७७ है। ये कुछ बातों में पुराणों जैसे हैं। इनमें सामान्यतः शिव-पार्वती का वार्तालाप है। इस वार्तालाप में कभी शिवजी पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कभी शिवजी के प्रश्नों का पार्वती उत्तर देती हैं। महानिर्वाण, कुलार्णव, कुलसार, प्रपंचसार, तन्त्रराज, रुद्रयामल, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल और तोडलतन्त्र महत्त्वपूर्ण शाक्त-आगम-ग्रन्थ हैं। आगमों में अनेक गुह्य तान्त्रिक अभ्यासों के बारे में बताया गया है। कुछ अभ्यास शक्ति प्रदान करते हैं तथा अन्य ज्ञान और मोक्ष। शक्ति भगवान् शंकर की सर्जक शक्ति है। शाक्तमत वास्तव में शैवमत का पूरक है।
आगमों पर उपलब्ध ग्रन्थों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है- ईश्वरसंहिता, अहिर्बुध्न्यसंहिता, सनत्कुमारसंहिता, नारद-पांचरात्र, स्पन्दप्रदीपिका और महानिर्वाणतन्त्र ।
षड्दर्शन
यह हिन्दू-ग्रन्थों के बौद्धिक अनुभाग हैं। प्रथम चार सहजानुभूत हैं तथा पाँचवाँ दर्शन उत्प्रेरक एवं भावनात्मक है। दर्शन वेदों पर आधारित विभिन्न मत हैं। आगम ईश्वरपरक हैं। दर्शन-साहित्य दार्शनिक है। दर्शन उन विद्वानों के लिए है जिनमें प्रतिभा, विवेक, तर्क करने की क्षमता तथा सूक्ष्म बुद्धि है। पुराण, इतिहास और आगम जन-साधारण के लिए हैं। दर्शन बुद्धि को प्रभावित करते हैं; पुराण, इतिहास आदि हृदय को।
दर्शन के छह अंग हैं (षड्दर्शन)। दर्शन का अर्थ है-किसी वस्तु या तथ्य को देखने की विधि। षड्दर्शन छह विभिन्न दर्शन-प्रणालियाँ या दर्शनिक मत हैं। दर्शनशास्र के छह मत सत्य के छह निरूपण (demonstration) हैं। प्रत्येक मत ने अपने ढंग से वेदों के विभिन्न भागों को विकसित किया है, क्रमबद्ध किया है तथा उनमें सह-सम्बन्ध स्थापित किया है। प्रत्येक विधि के एक सूत्रकार अर्थात् ऋषि हैं जिन्होंने उस मत के सिद्धान्तों को क्रमबद्ध करके उन्हें सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है।
सूत्र सारगर्भित तथा अल्पाक्षरिक हैं। ऋषियों ने सूत्रों में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। उनके भाष्यों की सहायता लिये बिना इन सूत्रों को समझना बड़ा कठिन है। कई भाष्यकारों ने उनके भाष्य किये हैं। बाद में मूल-भाष्यों की भी टिप्पणियाँ तथा भाष्य लिखे गये।
षड्दर्शन (अर्थात् षट्शास्त्र) हैं- गौतम ऋषि द्वारा प्रवर्तित न्याय, कणाद ऋषि का वैशेषिक, कपिल मुनि का सांख्य, महर्षि पतंजलि का योग, जैमिनि का पूर्वमीमांसा और बादरायण (व्यास) का उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्त। दर्शन-साहित्य तीन युग्मों में विभक्त है। इसकी शैली सूत्रात्मक है तथा इसमें वेदों के दर्शन को तकों की सहायता से समझाया गया है। ये युग्म हैं न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग, मीमांसा और वेदान्त।
सूत्र
स्वल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् ।
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः।।
सूत्र कम-से-कम अक्षरों की छोटी-सी रचना है जिसके लक्षण हैं जो अस्पष्ट न हो, जिसमें सन्देहास्पद अभिव्यक्ति न हो, जिसमें सम्पूर्ण अर्थ साररूप में समाया हुआ हो, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि न हो तथा जो अवरोध-रहित हो।
सूत्रकार कष्ट-कल्पित शब्दों तथा विचारों से युक्त दुर्बोध सूत्र में से यदि एक अक्षर भी कम करने में समर्थ होता है तो वह इतना हर्षित होता है कि जितना कोई पुत्र के जन्म पर। सूत्र-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ, अत्यन्त सारगर्भित और सर्वथा परिपूर्ण ग्रन्थ है-पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। पाणिनि समस्त सूत्रकारों के जनक हैं जिनसे उन सबने सूत्रों की रचना-विधि प्राप्त की है। सूत्रों का आशय है-ज्ञान के विशाल भण्डार को ऐसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना जिसे सदैव स्मरण रखा जा सके। छह वेदांगों तथा षड्दर्शन से विश्व के सूत्र-साहित्य के बारह समूह (sets) बनते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक उत्तरकालीन रचनाएँ भी हैं जैसे नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्यभक्तिसूत्र आदि।
भाष्य
सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः ।
स्वपदानि च वर्ण्यते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ।।
सूत्रों का शब्दशः अनुवाद, उनकी विस्तृत व्याख्या भाष्य है। भाष्य में भाष्यकार के व्यक्तिगत विचार भी सम्मिलित रहते हैं। संस्कृति-साहित्य में (दृष्टान्तयोग्य) सर्वोत्तम भाष्य पतंजलि द्वारा रचित पाणिनि के व्याकरण-सूत्रों का भाष्य है। यह भाष्य इतना प्रसिद्ध है कि यह महाभाष्य कहलाता है और इसका प्रसिद्ध लेखक महाभाष्यकार। पतंजलि भाष्यकारों के जनक हैं। दूसरा महत्त्वपूर्ण भाष्य है शाबर स्वामी द्वारा रचित मीमांसा-सूत्र पर लिखी व्याख्या। शाबर स्वामी ने पतंजलि से ही भाष्य-रचना सीखी। तीसरा महत्त्वपूर्ण भाष्य है ब्रह्मसूत्रों पर शंकर द्वारा लिखित भाष्य जो शाबर भाष्य से मिलता-जुलता है। भारतीय षड्दर्शन पर वात्स्यायन, प्रशस्तपाद, विज्ञानभिक्षु, व्यास, शाबर और शंकर द्वारा भाष्य लिखे गये थे। वेदान्त या ब्रह्मसूत्रों पर रामानुज, मध्व, वल्लभ, निम्बार्क आदि द्वारा लिखे गये लगभग १६ भाष्य हैं।
वृत्ति
सद्वृत्तिः सन्निबन्धना
सूत्र की संक्षिप्त परन्तु स्पष्ट व्याख्या को वृत्ति कहते हैं। यह भाष्य की तरह विस्तृत नहीं होती। ब्रह्मसूत्रों पर बोधायण की वृत्ति एक श्रेष्ठ ग्रन्थ है।
वार्त्तिक
उक्त नुक्तदुरुक्तानं चिन्ता यत्र प्रवर्तते।
तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुः वार्त्तिकज्ञ विचक्षणः ।।
वार्तिक वह रचना है जिसमें उन बातों की विवेचना होती है जिनको भाष्य में स्थान नहीं मिल पाता या जिनकी भाष्य में अपूर्ण व्याख्या की जाती है। इस अपूर्णता को दूर करने के लिए वार्तिक में कुछ आवश्यक तथ्य जोड़ दिये जाते हैं। वार्त्तिकों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं-पाणिनि के सूत्रों पर कात्यायन का वार्त्तिक, शंकर के उपनिषद्-भाष्यों पर सुरेश्वर की और कर्ममीमांस के शाबर-भाष्य पर कुमारिल भट्ट का वार्त्तिक।
व्याख्यान अथवा टीका
मूल बात की सहायता से सरल भाषा में समझाना व्याख्यान कहलाता है। व्याख्यान में (विशेषकर काव्य के व्याख्यान में) श्लोक के विश्लेषण की आठ विभिन्न विधियाँ प्रयुक्त होती हैं-जैसे पदच्छेद, विग्रह, सन्धि, अलंकार, अनुवाद आदि। संस्कृत-साहित्य-शास्त्र के अध्ययन का यह एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। अनुव्याख्यान (जैसा कि श्री मध्व द्वारा लिखा गया) पूर्व-लिखित रचना की अधिक विस्तृत पुनरुक्ति है। अनुवाद मूल दुरुह पाठ का पुनरुल्लेख है। टीका व्याख्यान का ही दूसरा नाम है। वाचस्पति मिश्र का व्याख्यान (विशेषकर शंकर के ब्रह्मसूत्र-भाष्य पर) सर्वश्रेष्ठ है।
टिप्पणी
टिप्पणी वृत्ति की भाँति है; किन्तु वृत्ति की अपेक्षा कम रूढ़िवादी है। यह मूल-पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों और पदों की व्याख्या मात्र है। उदाहरण है-पतंजलि के महाभाष्य पर कैयट की टिप्पणी पर नागेश भट्ट की टिप्पणी तथा वाचस्पति मिश्र की 'भामती' पर अमलानन्द की टिप्पणी पर अप्पय की टिप्पणी।
अन्य धर्मग्रन्थ
तेवारम तथा तिरुवाचकम (दक्षिण भारत के शैव सन्तों के भजन हैं), दक्षिण भारत के आलवार सन्तों के 'दिव्य प्रबन्धम्', कबीर के पद, तुकाराम के अभंग, तुलसीदास का रामचरितमानस -ये सब महान् आत्माओं के उद्गारों के रूप में उनके महान् ग्रन्थ हैं। इनमें वेदों का सार निहित है।
ऐहिक साहित्य
सुभाषित
सुभाषित गद्य या पद्य में लिखी गयी विद्वद्वाणी, उपदेश और कहानियाँ हैं। उदाहरणार्थ भर्तृहरि के तीन शतक, सुभाषित रत्न-भाण्डागार और सोमदेव भट्ट का कथासरित्सागर अथवा क्षेमेन्द्र की बृहत्कथामंजरी। पंचतन्त्र और हितोपदेश भी इसी श्रेणी के ग्रन्थ हैं।
काव्य
काव्य पद्म, गद्य या गद्य-पद्य की मिश्रित शैली में लिखी गयी अत्यन्त विद्वित्तापूर्ण रचना है। सर्वोपरि काव्य-रचनाएँ हैं-कालिदास का रघुवंश और कुमारसम्भव, भारवि का किरातार्जुनीयम्, माघ का शिशुपालवधम् और श्रीहर्ष का नैषधीयचरितम्। समस्त संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ गद्यकाव्य श्रेष्ठ संस्कृत के प्रतिभासम्पन्न लेखक बाण भट्ट ने लिखे, उदाहरण-कादम्बरी और हर्षचरितम् गद्य-पद्य में मिश्रित प्रसिद्ध रचनाएँ हैं- चम्पूरामायण और चम्पूभारत। ये सब उच्च कोटि की कृतियाँ हैं जो सदैव भारतवर्ष की साहित्यिक उपलब्धियों को उजागर करती रहेंगी।
नाटक
ये शैक्षिक नाटक हैं जिनमें शृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, वीभत्स और रौद्र रसों का सुन्दर परिपाक हुआ है। यह कहा जाता है कि नवें रस शान्त पर कोई नहीं लिख सकता। इसकी प्राप्ति कैवल्यावस्था में ही हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ नाटक कालिदास द्वारा रचित 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्', भवभूतिकृत 'उत्तर- रामचरितम्' और विशाखदत्तकृत 'मुद्रा-राक्षस' हैं।
अलंकार
अलंकारशास्त्र के इन ग्रन्थों के गद्य और पद्य-दोनों शैलियों की आलंकारिक भाषाओं की पूर्णता और सौन्दर्य के विज्ञान तथा सशक्त एवं ललित रचना से सम्बन्धित विवेचना है। ये संस्कृत साहित्य के मूल तत्त्व हैं तथा ये काव्य और नाटकों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। मम्मट का 'काव्यप्रकाश' और जगन्नाथ का 'रस-गंगाधर' सर्वोत्तम अलंकार-ग्रन्थ हैं।
उपसंहार
ये हैं समग्र संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थ। भारतीय संस्कृति एक वृक्ष है; श्रुति उस वृक्ष की जड़ है; स्मृति, इतिहास और पुराण तने हैं; आगम और दर्शन शाखाएँ हैं; सुभाषित, काव्य, नाटक और अलंकार इस भारतीय संस्कृति-वृक्ष के पुष्प हैं।
स्मृति, इतिहास, पुराण, आगम और दर्शन वेद के ही विकसित रूप हैं। उनका अन्तिम स्रोत वेद है। उन सबमें सामान्य लक्ष्य है-मानव को इस योग्य बनाना कि वह अपना अज्ञान समाप्त कर सके तथा ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा पूर्णता, स्वतन्त्रता, अमरता और परमानन्द की उपलब्धि कर सके। उनका यह भी लक्ष्य है कि मनुष्य ईश्वर के समान हो जाये, 'उससे' अभिन्न हो जाये।
तृतीय अध्याय
हिन्दू-धर्म के विविध रूप
धर्म के साकार रूप, धर्म के नियन्ता और संरक्षक तथा धर्म के मूल-स्रोत ईश्वर को मौन प्रणाम!
धर्म क्या है? धर्म अर्थात् जो धारण करे। एकमात्र धर्म ही लोगों को धारण करता है। धर्म शब्द 'धृ' धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना, और इसका शाब्दिक अर्थ है-वह जो इस विश्व को, विश्व के लोगों को, व्यष्टि से समष्टि-पर्यन्त अखिल सृष्टि को धारण करता है। यह परमेश्वर का शाश्वत दिव्य नियम है। समस्त सृष्टि का धारण-पोषण इसी सर्वशक्तिमान् दिव्य नियम द्वारा हो रहा है। इसलिए धर्म-पालन का आशय है-इन नियमों को समझ कर इनका पालन करना।
जो मनुष्य का कल्याण करे, वह धर्म है। धर्म इस विश्व का आधार है। धर्म व्यक्तियों की मर्यादा बनाये रखता है। जो सुरक्षा प्रदान करता है, वह धर्म है। धर्म शाश्वत सुख और अमरत्व का मार्ग प्रशस्त करता है।
जो धर्म है, वह वस्तुतः सत्य है; अतः जो सत्य बोलता है, वह धर्म को ही बोलता है तथा जो धर्म की बात करता है, वह सत्यवादी कहलाता है। दोनों एक ही वस्तु हैं।
मानव-चरित्र को विकसित करने वाले समस्त बाह्य कर्म तथा विचार और मानसिक अभ्यास भी धर्म के अन्तर्गत आते हैं। धर्म ईश्वर से उद्भूत होता है और आपको ईश्वर की ही ओर ले जाता है।
धर्म की परिभाषा
कोई भी भाषा पूर्ण नहीं है। संस्कृत शब्द 'धर्म' के लिए अँगरेजी में कोई समानार्थी शब्द नहीं है। धर्म की परिभाषा देना अत्यन्त कठिन है।
साधारणतया सदाचरण या कर्तव्य को धर्म कहा जाता है। धर्म सदाचरण का सिद्धान्त है। यह पवित्रता का सिद्धान्त है। यह एकता का भी सिद्धान्त है। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो द्वन्द्व को उत्पन्न करे, वह अधर्म है और जो द्वन्द्व का अन्त करके सामंजस्य लाये, वह धर्म है। जो भी सबको एकता के सूत्र में बाँध कर पवित्र दिव्य प्रेम एवं विश्व-भ्रातृत्व की भावनाओं को विकसित करने में सहयोग दे, वह धर्म है। जो भी विसंगति, फूट, असामंजस्य तथा घृणा को प्रोत्साहन दे, वह अधर्म है। जो भी विसंगति, फूट, असामंजस्य तथा घृणा को प्रोत्साहन दे, वह अधर्म है। धर्म सामाजिक जीवन को दृढ़ता प्रदान करता है तथा उसका पोषक है। धर्म के नियम सांसारिक कार्यकलापों का नियमन करने के लिए बनाये गये हैं। धर्म का पालन करने से इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। धर्म अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने का साधन है। यदि आप इसका उल्लंघन करेंगे, तो यह आपको जीवित नहीं रहने देगा। यदि आप इसकी रक्षा करेंगे, तो यह आपकी रक्षा करेगा। मृत्यूपरान्त भी धर्म आपका एकमात्र साथी है। मानवता का मात्र आश्रय धर्म ही है।
जो मनुष्य को ऊँचा उठाता है, वह धर्म है-यह एक अन्य परिभाषा है। धर्म वह है जो आपको पूर्णता के मार्ग पर अग्रसर करता है। धर्म ईश्वर के साथ साक्षात् सम्पर्क करने में आपकी सहायता करता है। धर्म आपको दिव्य बनाता है। धर्म ईश्वर के पास तक पहुँचाने वाला आरोही सोपान है। आत्म-साक्षात्कार सर्वोच्च धर्म है। धर्म हिन्दू-नीति-शास्त्र का सार है। ईश्वर धर्म का केन्द्र है।
धर्म का अर्थ है आचार अर्थात् दैनिक जीवन का नियमन। आचार सर्वोच्च धर्म है। यह तप का आधार है। यही समृद्धि, सौन्दर्य तथा दीर्घायु प्रदान करता है और वंश के नैरन्तर्य में सहायक होता है। दुराचार और अनैतिकता कुख्याति, दुःख, रोग और अकाल मृत्यु की परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। धर्म की जड़ें नैतिकता में हैं और धर्म के नियन्ता हैं स्वयं परमात्मा।
महर्षि जैमिनि के अनुसार-जो वेद-सम्मत हो और जो अन्त में दुःख का कारण नहीं बने, वह धर्म है।
वैशेषिक-दर्शन के अधिष्ठाता कणाद ऋषि ने वैशेषिक-सूत्रों में धर्म की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है : "यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस सिद्धिः सा धर्म:" -जिससे अभ्युदय (इहलोक) तथा निःश्रेयस (परलोक में दुःख का पूर्ण निवारण तथा शाश्वत सुख की उपलब्धि) की प्राप्ति हो, वह धर्म है।
वेदों की एकमात्र प्रामाणिकता
चारों वेद, स्मृतिग्रन्थ, उन लोगों का व्यवहार जो इन ग्रन्थों की मूल भावना को आत्मसात् करके उनके अनुसार आचरण करते हैं, पावन पुरुषों का चरित्र और मनुष्य की आत्म-तुष्टि-ये सब धर्म के आधार हैं।
धर्म के विषय में वेद ही अन्तिम प्रमाण हैं। वेद के अतिरिक्त ज्ञान के किसी स्रोत से धर्म के विषय में नहीं जाना जा सकता। धर्म के विषय में तर्क प्रमाण-सिद्ध नहीं हो सकता। विश्व के धर्मग्रन्थों में वेद प्राचीनतम हैं। समस्त सभ्य संसार के श्रेष्ठ विद्वान् और पुरावेत्ता इसका समर्थन करते हैं। वे एक स्वर से घोषित करते हैं कि किसी भी मानवीय भाषा में लिखे गये ग्रन्थों में ऋग्वेदसंहिता निःसन्देह प्राचीनतम है। कोई भी पुरावेत्ता ऋग्वेदसंहिता के रचना-काल अथवा इसके प्राकट्य की तिथि निश्चित नहीं कर पाया।
परिवर्तनशील धर्म
जिस प्रकार एक चिकित्सक विभिन्न रोगियों को उनकी प्रकृति और रोगों के अनुसार विभिन्न औषधियाँ सेवन करने का परामर्श देता है, उसी प्रकार हिन्दू-धर्म विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के कर्तव्य निर्धारित करता है। स्त्रियों के नियम पुरुषों के नियमों से भिन्न हैं। विभिन्न वर्गों और आश्रमों के नियमों में भी भेद हैं; किन्तु सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह आदि कर्तव्य सभी मनुष्यों के लिए हैं।
व्यक्ति की परिस्थिति, युग, कर्म-विकास का स्तर और उसके समुदाय के अनुरूप ही उसका धर्म होता है। इस शताब्दी का धर्म दशवीं शताब्दी के धर्म से भिन्न है।
समय की परिस्थितियों के अनुसार धर्म का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। आपद्धर्म भी सामान्य व्यवहार से इसी प्रकार का व्यतिक्रम है। इस प्रकार का व्यतिक्रम विषम विपत्ति-काल में ही अनुमत है।
किन्हीं परिस्थितियों में जो धर्म है, अन्य परिस्थितियों में वही अधर्म बन सकता है। यही कारण है कि धर्म का रहस्य अत्यन्त गहन और सूक्ष्म माना जाता है। गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा है-"कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र (धर्मग्रन्थ) ही प्रमाण हैं" (१६/२४)। धर्म का सत्य गुप्त रहता है। श्रुतियाँ और स्मृतियाँ बहुत हैं। सबके लिए सुप्रकाशित धर्म-मार्ग वह है जिस पर आत्मसाक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति चल चुके हैं।
अन्य धर्मों में धर्माचरण
अन्य सब धर्म भी धर्माचरण को महत्त्व देते हैं। बौद्ध, ईसाई, जैन, सिक्ख, पारसी और इस्लाम-सभी धर्म इसे महत्त्व देते हैं। अफलातून, सुकरात, अरस्तु, काण्ट, स्वीडनबर्ग, स्पिनोज़ा आदि ने नैतिकता, कर्तव्यपरायणता तथा सदाचार को बहुत महत्त्व दिया है तथा इन्हें जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन बताया है। प्रत्येक धर्म धर्माचरण के कतिपय पक्षों पर बल देता है।
धर्माचरण के लाभ
धर्मग्रन्थों में पुरुषार्थ-चतुष्टय-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। अकेला धर्म ही मोक्ष, अमरता, असीमित परमानन्द, परम शान्ति और सर्वोच्च ज्ञान का द्वार है। धर्म ही मुख्य पुरुषार्थ है। धर्माचरण के द्वारा ही आप समस्त मानवीय कर्मों के सर्वोच्च गौरव तथा समस्त अभीष्ट वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं।
धर्माचरण से ही जीवन के अन्तिम लक्ष्य, सर्वोच्च कल्याण अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होती है; आन्तरिक शान्ति, सुख और शक्ति का भी अनुभव होता है; जीवन पूर्णतः अनुशासित हो जाता है; शक्ति और क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है तथा वह अनुभव कर लेता है कि इन नाम और रूपों के पीछे एक ही सारतत्त्व तथा जीवन्त-सत्य विद्यमान है। धर्माचरण करने वाला व्यक्ति तत्त्वान्तरित हो जाता है। उसका स्वभाव ही परिवर्तित हो जाता है। वह परम तत्त्व के साथ एकाकार हो जाता है। वह ऊपर-नीचे, दायें-बायें, सामने-पीछे, भीतर-बाहर और अखिल विश्व में ब्रह्म को व्याप्त देखता है।
धर्म के भेद
धर्म दो प्रकार का होता है : (१) सामान्य अथवा सार्वभौमिक, तथा (२) विशेष अथवा व्यक्तिगत। सन्तोष, क्षमा, आत्मनिग्रह, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, सत्यासत्य तथा सदसत्-विवेक, तत्त्वज्ञान और अक्रोध सार्वभौमिक धर्म के अन्तर्गत हैं। ये मनु के अनुसार धर्म की दश विशेषताएँ हैं। वर्णाश्रम-धर्म विशेष धर्म है।
धर्म के विभिन्न प्रकार हैं-सनातन धर्म, सामान्य-धर्म, विशेष-धर्म, वर्णाश्रम-धर्म, स्व-धर्म, युग-धर्म, कुल-धर्म, मानव-धर्म, पुरुष-धर्म, स्त्री-धर्म, राज-धर्म, प्रजा-धर्म, प्रवृत्ति-धर्म और निवृत्ति-धर्म।
सनातन-धर्म
सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत-धर्म, प्राचीन नियम। यह वेदों पर आधारित है। यह प्रचलित धमों में प्राचीनतम है। हिन्दू-धर्म ही सनातन धर्म है। वेदों में जिसे परमार्थ या अन्तिम मोक्ष का साधन घोषित किया गया है, वह सनातन धर्म अथवा हिन्दू-धर्म है।
सनातन धर्म की आधारशिला श्रुति है, स्मृतिग्रन्थ इसकी भित्तियाँ हैं तथा पुराण-इतिहास इसके स्तम्भ हैं। प्राचीनकाल में श्रुतियाँ मौखिक याद की जाती थीं। गुरु शिष्य को गा कर सुनाते थे और शिष्यगण उनका अनुसरण करते हुए उन्हें गाते थे। वे लिखित नहीं थीं। समस्त मत तथा दर्शन-पद्धतियाँ श्रुति को अन्तिम प्रमाण मानती हैं। श्रुति के पश्चात् स्मृति को प्रामाणिक माना जाता है।
अपने दर्शन की गहनता तथा श्रेष्ठता की दृष्टि से हिन्दू-धर्म अद्वितीय है। इसके नैतिक उपदेश उदात्त, अनुपम और उत्कृष्ट हैं। इसे प्रत्येक मानवीय आवश्यकता के अनुकूल बनाया जा सकता है। यह धर्म स्वयं में एक पूर्ण धर्म है। इसे किसी अन्य धर्म से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। किसी अन्य धर्म ने इतने महान् सन्तों, योद्धाओं तथा पतिव्रताओं को जन्म नहीं दिया। आप इसके बारे में जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसके प्रति आपके श्रद्धा और प्रेम उतने ही अधिक बढ़ेंगे। आप जितना अधिक इसका अध्ययन करेंगे, उतना अधिक यह आपको प्रबोध तथा तोष प्रदान करेगा।
भारतवर्ष-धर्मो का आवास
संसार का धार्मिक इतिहास बतलाता है कि अनादिकाल से भारतवर्ष महान् सन्तों, द्रष्टाओं और ऋषियों का आवास रहा है। मनुष्यों के चरित्र का निर्माण करने वाले समस्त महान् धार्मिक आदर्श, मानवता को दिव्य गौरव की पराकाष्ठा पर पहुँचाने वाले सदाचरण और नीति के सर्वोच्च सिद्धान्त और आध्यात्मिकता के समस्त दिव्य सत्य जिन्होंने मानव को दिव्य बना कर राष्ट्रों, आध्यात्मिक आदशों तथा मानव-समाज के उद्धारकों को एक दिशा प्रदान की-ये सब सर्वप्रथम भारत में ही उदित हुए। भारतवर्ष का आध्यात्मिक क्षितिज सदा उपनिषद्-ज्ञान के स्वतः देदीप्यमान सूर्य के तेज से ज्योतित रहा है। जब कभी विश्व के किसी भाग में महापरिवर्तन हुआ है, उसका मूल-कारण भारत के किसी भाग में किसी महान् आत्मा के अवतरण द्वारा उत्पन्न आध्यात्मिकता की लहरें रहा है।
हिन्दुओं की संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक स्वर्णयुग अन्य देशों की संस्कृति आदि की तुलना में अत्यन्त प्राचीन है। ईश्वर ने भारतवर्ष के ऋषि, योगी, महात्मा, आलवार, पैगम्बर, आचार्य, संन्यासी और सन्तों के माध्यम से सांसारिक प्राणियों में वार्तालाप किया। निश्चय ही उनके उपदेश तथा पुराणग्रन्थ ईश्वरप्रेरित हैं। ईश्वर एकमात्र प्रकाश और सत्य है जिससे समस्त धर्मों के उपदेश निःसृत होते हैं।
भारतवर्ष धर्मों का आवास है। इसका भक्ति और ईश्वरपरायणता में गौरवशाली स्थान है। यह योगियों तथा सन्तों के लिए प्रसिद्ध है। भारतवर्ष का लक्ष्य है आत्मदर्शन अर्थात् वैराग्य के द्वारा भागवती चेतना की प्राप्ति। भारतवर्ष का इतिहास धर्म का इतिहास है। इस देश की सामाजिक नियमावली धर्म पर आधारित है। योग, धर्म और धार्मिक नियमों से विरहित भारत का चित्र वैसा नहीं होगा जैसा कि वह सहस्रों वर्षों से रहा है। कुछ हिन्दू अभी तक सनानत-धर्म की विशिष्टताओं से परिचित नहीं हैं। यदि प्रत्येक हिन्दू जानता और समझता कि हिन्दू-धर्म क्या है, तो आज के हिन्दू इस धरती के देवता बन जाते।
ईश्वर करे, आप सब सनानत-धर्म-सम्बन्धी ज्ञान से विभूषित हों! ईश्वर करे, आप सब इस शाश्वत-धर्म की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील हों! भगवत्कृपा से आप सबके समक्ष हस्तामलक के समान सनातन धर्म के रहस्य प्रकट हों! आप सबको ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हो! वेद और सनातन धर्म की जय हो! समस्त वेदों और सनातन धर्म के स्रोत ब्रह्म की जय हो!
सामान्य-धर्म
प्रत्येक धर्म का एक सामान्य रूप होता है और दूसरा विशेष रूप। सामान्य रूप सदा-सर्वदा एक-सा रहता है। यह किसी परिस्थिति में नहीं बदलता। इस पर समय, स्थान तथा परिवेश के परिवर्तन और व्यक्तिगत विशिष्टताओं का प्रभाव नहीं पड़ता। धर्म का यह पक्ष सनातन अथवा शाश्वत कहलाता है। जो समय, स्थान और परिवेश के अनुरूप बदलता है, वह धर्म का बाह्य पक्ष अर्थात् कर्मकाण्ड है।
सामान्य-धर्म सब मनुष्यों का धर्म है। वर्णाश्रम-धर्म विशिष्ट धर्म है जिसका पालन जीवन की विशिष्ट अवस्थाओं में तथा विशेष जातियों के द्वारा किया जाता है। सामान्य-धर्म का पालन सभी वर्णों-आश्रमों के व्यक्तियों तथा विभिन्न पन्थों के अनुयायियों द्वारा किया जाना चाहिए। परोपकारिता किसी एक जाति या समुदाय की सम्पत्ति नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के पास यह गुण होना चाहिए।
धर्म के मौलिक सिद्धान्त
विष्णुसंहिता के अनुसार क्षमा, सत्य, मन का निग्रह, शुचिता, दानशीलता, इन्द्रिय-निग्रह, अहिंसा, गुरु-सेवा, तीर्थयात्रा, दया, सरलता, अलोभ, देव और ब्राह्मणों की उपासना और अद्वेष सामान्य-धर्म के संघटक तथा सब मनुष्यों द्वारा पालन करने योग्य (धर्म के) नियम हैं।
महाभारत के अनुसार श्रद्धा, तपश्चर्या, सत्य, अक्रोध, एकपत्नी-व्रत, शुचिता, विद्या, अनसूया, आत्मज्ञान और सहिष्णुता धर्म के मौलिक सिद्धान्त हैं।
पद्मपुराण में कहा गया है कि इन्द्रिय-निग्रह, सत्य, तप, दान, आत्म-संयम, सहिष्णुता, पवित्रता, अहिंसा, शान्ति और अस्तेय से धर्म का प्रादुर्भाव होता है और ये दश गुण धर्म की पहचान हैं। इस पुराण के अनुसार योग्य व्यक्तियों को उपहार देना; भगवान् श्रीकृष्ण पर अपने विचारों को संकेन्द्रित करना; माता-पिता की भक्ति करना, नित्य के भोजन का अंश सब जीवों को देना और गौ को ग्रास देना-ये धर्म के लक्षण हैं।
मत्स्यपुराण के अनुसार अद्वेष, अपरिग्रह, इन्द्रिय-संयम, तप, ब्रह्मचर्य, करुणा, सत्य, सहिष्णुता और धैर्य सनातन धर्म के मौलिक मूल-तत्त्व हैं।
राजयोगदर्शन के प्रतिपादक पतंजलि महर्षि का कथन है कि निम्नांकित दश गुणों का पालन सभी को करना चाहिए। प्रथम पाँच हैं-अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य (विचार, वाणी और कर्म में), अस्तेय और अपरिग्रह। ये यम हैं। अन्य पाँच गुण हैं-शौच (आन्तरिक तथा बाह्य शुद्धि), सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान। ये नियम हैं।
गीता में निम्नांकित गुणों को दैवी सम्पदा की संज्ञा दी गयी है-निर्भयता, अन्तःकरण की स्वच्छता, तत्त्वज्ञान के लिए ध्यानयोग में दृढ़ स्थिति, दान, इन्द्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, शरीर-इन्द्रियों सहित अन्तःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कर्तृत्व-अभिमान का त्याग, शान्ति, निन्दादि न करना, जीवों के प्रति दया, अलोलुपता, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शुचिता, अद्रोह तथा पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब गुण इन चार मूलभूत गुणों की अभिव्यक्ति है- (१) सत्य, (२) अहिंसा, (३) शुचिता और (४) आत्मसंयम। बौद्धमत के अष्टम-मार्ग तथा भगवान् यीशु के 'सरमन आन द माउण्ट' के सन्दर्भ में जिन गुणों की चर्चा की गयी है, वे भी उपर्युक्त मूलभूत गुणों के ही अन्तर्गत हैं।
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने के लिए गुणों को विकसित करना अपरिहार्य है। ब्रह्म शुचिता है। शाश्वत ब्रह्म शुचिता के अभाव में नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्म सत्य है। शाश्वत ब्रह्म सत्य के अभ्यास के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्म निर्भयता है। जब तक आप सर्वथा निर्भय न हो जायें, आप शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर के प्रति आसक्ति भय तथा देहाध्यास को जन्म देती है। यदि आप निर्भय हो जायें, तो अपने को शरीर मान लेने का भाव समाप्त हो जायेगा।
लोभ, कृपणता, क्रूरता और धृष्टता से आपने अपने हृदय को चकमक, लोहे अथवा हीरे से भी अधिक कठोर बना लिया है। दया, सहानुभूति, दान, वदान्यता, उदारता, अनपकार, सौम्यता, निःस्वार्थ कर्म और दीन-दुःखियों की सेवा द्वारा आप उसे कोमल बना सकते हैं। मिथ्याचार, असत्य और (पिशुनता) चुगलखोरी द्वारा आपने अपने हृदय को कुटिल तथा संकीर्ण बना लिया है। आर्जव, सच्चाई, शुचिता, दान और अलोलुपता हृदय को विकसित कर सकते हैं। आपने कामुकता के कारण हृदय को अपवित्र कर दिया है। मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य के अभ्यास द्वारा उसे आप परिशुद्ध कर सकते हैं।
अहिंसा
अहिंसा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुण है। महर्षि पतंजलि ने इसे यमों में प्रथम स्थान दिया है। अहिंसा का अभ्यास मन, वाणी और कर्म से होना चाहिए। अहिंसा का अभ्यास कायरता या दुर्बलता नहीं है। यह सर्वोच्च श्रेणी की वीरता है। इसके अभ्यास के लिए असीम धैर्य, सहिष्णुता, अनन्त आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति और प्रबल इच्छा-शक्ति आवश्यक है।
अहिंसा सत्य की ही अभिव्यक्ति अथवा उसका रूपान्तरण है। सत्य और अहिंसा सदा साथ-साथ रहते हैं। जो अहिंसा में संस्थित हो गया है, वह विश्व को हिला सकता है। उसकी उपस्थिति में वैरभाव लुप्त हो जाता है, शेर और गाय, सर्प और नेवला शान्तिपूर्वक साथ-साथ रहने लगते हैं।
हिन्दू, बौद्ध और जैन-मतों में अहिंसा पर बहुत बल दिया जाता है। भगवान् यीशु ने 'शैलोपदेश' (Sermon on the Mount) में अहिंसा पर बहुत बल दिया है। वह कहते हैं-"यदि कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दें।"
जो अहिंसा में भली प्रकार स्थित है, वही आत्मसाक्षात्कार करने की आशा कर सकता है। जो अहिंसा का अभ्यास करता है, उसमें दिव्य विश्व-प्रेम अत्यधिक विकसित हो जाता है। अहिंसा का अभ्यास करने से अन्ततोगत्वा ब्रह्म से तादात्म्य भाव स्थापित हो जाता है। अहिंसक मनुष्य ही आत्मसंयम कर सकता है। प्रतिशोध-खून का बदला खून-आसुरी प्रकृति के व्यक्ति का सिद्धान्त है। यह पाशविक प्रकृति है। परन्तु बुराई के बदले भलाई करना दिव्यता है। अहिंसा के अभ्यासी को निरन्तर जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि किंचित् भी असावधानी हो गयी तो आप पूर्व के बुरे संस्कार और आवेगों के प्रभाव में आ जायेंगे तथा न चाहते हुए भी हिंसा के प्रभाव में आ जायेंगे।
सत्य
ब्रह्म 'सत्' है। सत्य का पालन मन, वाणी और कर्म से करना चाहिए। यदि आप सत्य में स्थित हों, तो अन्य समस्त गुणों से आप स्वतः ही विभूषित हो जायेंगे। राजा हरिश्चन्द्र ने सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी कारण वह अब भी अमर हैं। युधिष्ठिर भी सत्य के पुजारी थे। सत्य से बड़ा अन्य कोई गुण नहीं है। सत्य और अहिंसा नैतिक जीवन का मुकुट और गौरव हैं। तैत्तिरीय उपनिषद् में गुरु अपने दीक्षान्त-भाषण में शिष्यों से कहता है- "सत्यं वद" अर्थात् सत्य बोलो। संसार की जड़ें सत्य में हैं। धर्म की जड़ें सत्य में हैं। समस्त धर्मों की जड़ें भी सत्य में हैं। ईमानदारी, न्यायप्रियता, आर्जव तथा निष्कपटता सत्य की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं।
शुचिता
शुचिता का तात्पर्य है बाह्य और आन्तरिक अर्थात् शारीरिक और मानसिक शुद्धि। मन को शुद्ध करने के लिए पहले शरीर को शुद्ध करना पड़ता है।
शरीर भगवान् का मन्दिर है। नित्य स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहन कर इसे शुद्ध रखना चाहिए। स्वच्छता ईश्वरपरायणता का एक अंग है। मन को शुद्ध रखने के लिए भोजन पर नियन्त्रण रखना आवश्यक माना गया है
भोजन का मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सात्त्विक और पवित्र भोजन मन को पवित्र बनाता है। भोजन के सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्म सारतत्त्व से ही मन बनता है; इसलिए, जैसा भोजन होगा, वैसा ही मन बनेगा।
आपको मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। आपका हृदय स्फटिक अथवा हिमालय की बर्फ की भाँति शुद्ध होना चाहिए; तभी दिव्य ज्योति अवतरित होगी। स्पष्टवादिता, निष्कपटता, आर्जव तथा सब प्रकार के अवगुणों का अभाव शुचिता के ही अन्तर्गत है। जो शुचि (शुद्ध) है, उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना अत्यन्त सरल है।
आत्मसंयम
आपको पूर्ण आत्मसंयम रखना चाहिए। आत्मसंयम से तात्पर्य है-शरीर और मन दोनों पर नियन्त्रण। आत्मसंयम का आशय आत्मपीड़न नहीं है। आपको नियमित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए। आपको अपनी समस्त इन्द्रियाँ अपने नियन्त्रण में रखनी चाहिए। इन्द्रियाँ उपद्रवी तथा निरंकुश घोड़ों के समान हैं। शरीर रथ है। मन लगाम है। बुद्धि रथी तथा आत्मा इस रथ का स्वामी है। यदि इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण न रखा जाये, तो वे इस रथ को अगाध गर्त में गिरा देंगी। आप बरबाद हो जायेंगे। जो व्यक्ति लगाम को दृढ़ रख कर बुद्धिमत्ता से घोड़ों (इन्द्रियों) पर नियन्त्रण रखता हुआ रथ हाँकता है, वह कुशलतापूर्वक अपनी मंजिल (मोक्ष अथवा शाश्वत परमानन्द के धाम) तक पहुँच जायेगा।
आत्मसंयम का अर्थ है-आत्म-बलिदान, अहंकार का नाश, धैर्य, क्षमा, सहिष्णुता तथा नम्रता। वैराग्य के द्वारा राग पर विजय प्राप्त करें। विषयपरायण जीवन के दोषों-जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, पीड़ा, दुःख आदि पर ध्यान देने से (दोष-दृष्टि या मिथ्या-दृष्टि रखने से) आपके मन में वैराग्य का उदय होगा। क्षमा, प्रेम और निःस्वार्थ सेवा द्वारा क्रोध तथा घृणा पर विजय प्राप्त करें। बुराई को भलाई द्वारा जीतें। बुराई के बदले भलाई करें। कामुकता को ब्रह्मचर्य और नियमित जप तथा ध्यान के अभ्यास द्वारा जीतें। लोभ को दान, उदारता और निष्काम कर्म के द्वारा जीतें। अभिमान को नम्रता द्वारा, भ्रम को विवेक और जिज्ञासा द्वारा जीतें। ईर्ष्या को उदारता, विशालता, आत्मभाव और श्रेष्ठता द्वारा जीतें। अहंभाव को आत्मबलिदान, आत्मसमर्पण, आत्मत्याग तथा अद्वैत, शाश्वत, आत्मदीप्त, आन्तरिक शासक, अन्तरात्मा अमर ब्रह्म के द्वारा जीतें।
आप सब धर्म के आधारभूत सद्गुणों को अपना कर (सामान्य-धर्म का पालन करके) शाश्वत परमानन्द और अमरता को प्राप्त करें।
वर्णाश्रम-धर्म
वर्णाश्रम-धर्म का सिद्धान्त हिन्दू-धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों में से एक है। वर्णाश्रम-प्रथा हिन्दुओं की विशिष्टता है। यह हिन्दू-धर्म का विशेषता-सूचक गुण है। यह गुण-कर्म के अनुसार अखिल विश्व में प्रचलित है, यद्यपि कोई विशेष नाम इस प्रकार के भेद को कहीं और नहीं दिया गया है।
विभिन्न जातियों के कर्तव्यों को वर्ण-धर्म कहते हैं। चार जातियाँ हैं-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जीवन की अवस्थाओं के कर्तव्य आश्रम-धर्म कहलाते हैं। चार आश्रम हैं-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
सिद्धान्त
मानव-समाज एक विशाल यन्त्र के समान है। व्यक्ति और जातियाँ इसके पुरजे हैं। यदि पुरजे कमजोर और टूटे हुए हों, तो यन्त्र काम नहीं कर सकता। पुरजों से रहित यन्त्र कुछ नहीं है। मानव शरीर सुचारु रूप से तभी काम कर सकता है, जब उसके अंग स्वस्थ तथा बलवान् हों। यदि शरीर के किसी भाग में पीड़ा हो, यदि उसका कोई अंग हो, तो मानव-यन्त्र बिगड़ जायेगा और अपना सामान्य कार्य नहीं करेगा।
यही दशा मानव-समाज की है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन भली प्रकार करना चाहिए। हिन्दू-ऋषि-मुनियों ने वर्णाश्रम-धर्म के नाम से सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श जीवन व्यतीत करने की एक योजना बनायी। हिन्दुत्व वर्णाश्रम-धर्म पर आधारित है। हिन्दू-समाज का ढाँचा वर्णाश्रम-धर्म पर टिका हुआ है। वर्णाश्रम-धर्म का पालन करके मनुष्य अपने क्रम-विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यह धर्म अपरिहार्य है। यदि नियमों का उल्लंघन किया जाये, तो समाज शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा।
वर्णाश्रम-धर्म का लक्ष्य है सार्वभौमिक और शाश्वत धर्म का विकास। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। यदि आप उसे नष्ट करते हैं, तो वह भी आपको नष्ट कर देगा। इसलिए अपने धर्म को कभी नष्ट न करें। यह सिद्धान्त जितना व्यक्ति के लिए सत्य है, उतना ही एक राष्ट्र के लिए। धर्म ही राष्ट्र को जीवित रखता है। धर्म ही मनुष्य की आत्मा है। धर्म एक राष्ट्र की भी आत्मा है।
पाश्चात्य देशों में और सम्पूर्ण जगत् में वर्णाश्रम-धर्म है, यद्यपि इसका वहाँ दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता है। कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों ने तीन श्रेणियों में मानव-समाज को विभाजित किया है-दार्शनिक, योद्धा और जनसाधारण। दार्शनिक ब्राह्मणों के सदृश हैं। इसी प्रकार योद्धा क्षत्रिय के तथा जनसाधारण वैश्य और शुद्र के सदृश हैं। समाज को पूर्णरूपेण व्यवस्थित रूप देने के लिए यह पद्धति अनिवार्य है।
चार जातियाँ
ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में हिन्दू-समाज के चार भागों में विभाजन का उल्लेख है। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण सृष्टिकर्ता परमात्मा के मुख से निकले, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से।
यह विभाजन गुण और कर्म के अनुसार किया गया है। गुण और कर्म से मनुष्य की जाति निर्धारित होती है। गीता (४/१३) में भगवान् श्रीकृष्ण ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है। वह कहते हैं- "गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गये हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अकर्ता, अविनाशी परमेश्वर को ही जानो।"
गुण तीन प्रकार के होते हैं-सत्त्व, रजस् और तमस्। सत्त्व श्वेत है; रजस् लाल और तमस् काला है। ये तीनों गुण मनुष्य में विभिन्न अनुपात में पाये जाते हैं। जिन लोगों में सत्त्व की प्रधानता होती है, वे ब्राह्मण हैं। वे बुद्धिमान् तथा विचारक होते हैं। वे शासकों का पथ-प्रदर्शन करने वाले पुजारी, मन्त्री अथवा दार्शनिक होते हैं। कुछ लोगों में रजस् की प्रधानता होती है, वे क्षत्रिय हैं। वे योद्धा अर्थात् कर्मशूर व्यक्ति होते हैं। वे शत्रु अथवा आक्रामकों से युद्ध करके देश की रक्षा करते हैं। कुछ व्यक्तियों में तमस् की प्रधानता होती है। वे वैश्य अर्थात् व्यापारी हैं। वे व्यापार तथा कृषि द्वारा धनोपार्जन करते हैं। शूद्र सेवक हैं। उनमें इनमें से कोई भी गुण अधिक विकसित नहीं है। वे अन्य जातियों की सेवा करते हैं।
व्यापक अर्थ में सात्त्विक पुरुष, जो पवित्र और सद्गुणी है तथा दिव्य जीवन व्यतीत करता है, ब्राह्मण है। वीरोचित गुणों से युक्त राजसी व्यक्ति क्षत्रिय है। व्यापारिक प्रवृत्ति वाला राजसी पुरुष वैश्य है। तामसी पुरुष शूद्र है। हिटलर और मुसोलिनी क्षत्रिय थे। फोर्ड वैश्य थे।
शान्ति, आत्मसंयम, तप, शुचिता, क्षमाशीलता, आर्जव, ज्ञान, आत्मदर्शन तथा ईश्वर में विश्वास-ये ब्राह्मण के प्रकृतिजात गुण हैं। पराक्रम, भव्यता, दृढ़ता, दक्षता और युद्ध से न भागना, उदारता और गर्व क्षत्रिय के प्रकृतिजात गुण हैं। इसी प्रकार कृषि, पशुपालन और व्यापार वैश्यों के प्रकृतिजात गुण हैं। सेवा-भाव शुद्र का प्रकृतिजात गुण है।
आध्यात्मिक अर्थशास्त्र का नियम
जाति-प्रथा अर्थात् वर्ण-धर्म में श्रम-विभाजन का सिद्धान्त निहित है। ऋषियों ने मानवीय प्रकृति का भली प्रकार अध्ययन किया था। वे इस परिणाम पर पहुँचे किं सब मनुष्य सब प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने यह आवश्यक ने कि सब विभिन्न वगों के लोगों को उनकी प्रवृत्ति, योग्यता अथवा गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिये जायें। ब्राह्मणों को आध्यात्मिक और बौद्धिक कायर्यों को सम्पन करने का उत्तरदायित्व दे दिया गया। राजनैतिक प्रशासन और सुरक्षा-कार्य क्षत्रियों को दिया गया। वैश्यों को राष्ट्र की खाद्य की आपूर्ति करने तथा आर्थिक व्यवस्था करने के काम सौंपे गये। शूद्रों को दासोचित कार्य सौंपे गये। ऋषियों ने हिन्दू-जाति की इन समस्त आवश्यकताओं को समझ कर वर्ण और आश्रम की प्रथा प्रचलित की थी।
यह श्रम-विभाजन वैदिक युग में आरम्भ हुआ। वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क है, क्षत्रिय उसकी भुजा है, वैश्य पेट है और शूद्र चरण है।
एक बार मन, प्राण और इन्द्रियों में इस बात को ले कर झगड़ा हुआ कि कौन बड़ा है। विभिन्न अंगों और पेट के बीच भी झगड़ा हुआ। यदि हाथ पेट से झगड़ा करने लगे, तो समस्त शरीर को कष्ट होगा। यदि प्राण शरीर से निकल जायें, तो सभी अंग निष्क्रिय हो जायेंगे। शिर अथवा पेट हाथ-पाँवों से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकते। यदि विभिन्न जातियों में यह झगड़ा हो कि कौन बड़ा है, तो समस्त सामाजिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हो जायेगा। सर्वत्र असामंजस्य, सम्बन्ध-भंग तथा मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। समाज के संचालन के लिए एक भिश्ती या नाई का उतना ही महत्त्व है जितना कि मन्त्री का। सामाजिक भवन आध्यात्मिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त पर खड़ा हुआ है। श्रेष्ठता या हीनता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी-अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार जनकल्याण अर्थात् विश्व-एकात्मता में योगदान देता है। यहाँ ऊँच-नीच का कोई प्रश्न नहीं उठता।
चरित्र से जाति-निर्णय
ब्राह्मण यदि अपवित्र, चरित्रहीन, दुराचारी तथा अनैतिक है, तो वह ब्राह्मण नहीं है। शूद्र यदि पवित्र और सद्गुणी है, तो वह ब्राह्मण है। विदुर कितने महान् थे! सत्यकाम जाबाल्य कितना महान् स्पष्टवादी तथा सीधा-सच्चा विद्यार्थी था। जाति का सम्बन्ध चरित्र से है। वर्ण का अर्थ त्वचा का रंग नहीं है; वर्ण है चरित्र या गुण का रंग। चरित्र और आचरण भी महत्त्वपूर्ण हैं, मात्र वंश-परम्परा ही नहीं। यदि कोई जन्म से ब्राह्मण है तथा साथ-ही-साथ उसमें ब्राह्मण के गुण भी हैं, तो यह अच्छी स्थिति है; क्योंकि कुछ गुण-सम्बन्धी योग्यताएँ ही ब्राह्मण का जन्म निर्धारित करती हैं।
जाति-प्रथा के लाभ और हानि
कई विदेशी आक्रमणों के बावजूद हिन्दू-धर्म जाति-व्यवस्था के कारण ही जीवित है; परन्तु जाति-व्यवस्था के कारण उनमें द्वेष और घृणा की भावनाएँ भी उत्पन्न हुई हैं। उनमें सहयोग की भावना नहीं है। यही कारण है कि वे आज निर्बल और बिखरे हुए हैं। व्यवस्था के नाम पर वे साम्प्रदायिक हो गये हैं। इसी कारण भारत की हो रही है।
जाति-व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है। यह नितान्त त्रुटि-रहित व्यवस्था है; किन्तु इसमें बाह्य कारणों से दोष उत्पन्न हो गये हैं। वर्ग अपने-अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने लगे। योग्यता और चरित्र की कसौटी धीरे-धीरे लुप्त होने लगी। जाति का निर्धारण जन्म से होने लगा। समस्त जातियाँ अपने आदशों से च्युत हो गयीं और कर्तव्यों को भूल बैठीं। ब्राह्मण स्वार्थी हो गये और उपर्युक्त योग्यता प्राप्त किये बिना अपने जन्म के ही बल पर अपने को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझने लगे। क्षत्रियों ने अपना शौर्य खो दिया। वैश्य लोभी बन गये। वे गलत साधनों से धनोर्पाजन करने लगे। वे लोगों के आर्थिक कल्याण का भी ध्यान नहीं रखते थे। दान देने और त्याग करने की भावना समाप्त हो गयी। शूद्र सेवा करने से कतराने लगे। वे बड़े अधिकारियों की तरह व्यवहार करने लगे। वे इस बात की अपेक्षा करने लगे कि दूसरे व्यक्ति उनकी सेवा करें। मानव के लोभ और अभिमान ने असंगति तथा असामंजस्य की स्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं।
वर्णाश्रम-धर्म में कोई बुराई नहीं है। मनुष्य के अहंकार और दम्भ ने समस्याएँ उत्पन्न की हैं। मनुष्य अथवा क्षुद्र जीव अपूर्ण है। उनमें दोष-ही-दोष हैं। वह केवल दूसरों से ऊँचा कहलाने का अधिकार प्राप्त करने की प्रतीक्षा में रहता है। ब्राह्मण सोचता है कि अन्य तीन जातियाँ उससे नीची हैं। क्षत्रिय सोचता है कि वैश्य और शूद्र उससे हीन हैं। इसी तरह एक धनिक शूद्र सोचता है कि वह निर्धन ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय से श्रेष्ठ है।
वर्तमान काल में वर्णाश्रम-धर्म नाम मात्र को जीवित बचा है। इसको भली प्रकार व्यवस्थित करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो अपने आदर्शों से च्युत हो चुके हैं और जो भली प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने-अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षा-दीक्षा उपयुक्त ढंग से होनी चाहिए। उन्हें अपने आद्य उच्च स्तर के अनुरूप स्वयं को उठाना चाहिए। साम्प्रदायिक भावना समाप्त हो जानी चाहिए। प्रेम, भक्ति, सहयोग, त्याग तथा सेवा की भावनाओं से ओत-प्रोत उन्हें एक नये मानस का विकास करना चाहिए।
चार आश्रम
जीवन में चार आश्रम अथवा अवस्थाएँ होती हैं। इनके नाम हैं-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक आश्रम के अपने-अपने कर्तव्य हैं। इन आश्रमों से मानव के क्रम-विकास में सहायता मिलती है। क्रम से चारों आश्रमों का जीवन व्यतीत करते हुए, मनुष्य अपनी पूर्णता तक पहुँचता है। प्रारम्भ से ले कर अन्त तक उसके जीवन का नियमन हो जाता है। प्रथम दो आश्रम प्रवृत्ति-मार्ग (कर्म-मार्ग) से सम्बन्धित हैं तथा अन्तिम दो (वानप्रस्थ और संन्यास) निवृत्ति-मार्ग (त्याग-मार्ग) से।
सुव्यवस्थित आध्यात्मिक क्रमविकास की ओर
सनातन धर्म में जीवन अत्यन्त क्रमिक रूप से व्यवस्थित है। इसमें मानवीय कार्यकलापों के विभिन्न पक्षों के विकास का पूर्ण अवसर रहता है। जीवन के प्रत्येक आश्रम के लिए उपयुक्त कर्मों तथा प्रशिक्षणों का निर्धारण कर दिया जाता है। जीवन एक महान् पाठशाला है जिसमें मानव के सामर्थ्य, क्षमताओं तथा मनःशक्तियों का क्रमशः विकास होता है।
प्रत्येक मनुष्य को क्रमिक रूप से विभिन्न आश्रमों में प्रवेश करना चाहिए। उसे किसी आश्रम में समय से पूर्व अपरिपक्व मनःस्थिति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक अवस्था को पूर्ण करने के पश्चात् ही वह अगले स्तर में प्रवेश कर सकता है। प्रकृति में विकास क्रमिक होता है, अनायास नहीं।
मनु ने स्मृति में कहा है- "जो ब्रह्मचर्य-आश्रम में रहता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत भंग किये बिना समस्त वेदों को अथवा कम-से-कम एक या दो वेदों का अध्ययन कर ले, वह गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश कर सकता है। जब गृहस्थ अपनी त्वचा में झुर्रियाँ या अपने केशों में सफेदी देख ले, अपने पौत्र का मुख देख ले, तब उसे वन में चले जाना चाहिए। वन में जीवन का तृतीय भाग (आश्रम) व्यतीत करने के पश्चात् उसे समस्त आसक्तियों को त्याग करके जीवन के चतुर्थ आश्रम में एक तपस्वी की भाँति भ्रमण करना चाहिए।”
हाँ, विशिष्ट परिस्थितियों में जीवन की किसी अवस्था (आश्रम) को छोड़ा ४६ जा सकता है। शुक जन्मजात संन्यासी थे। शंकर ने गृहस्थ- आश्रम में प्रवेश किये किस संन्यास ले लिया। कभी-कभी अति विशिष्ट परिस्थितियों में ब्रह्मचारी को भी संन्द ग्रहण करने की आज्ञा मिल जाती है; क्योंकि संसार के प्रति अपने ऋणों से पूर्व-जन्म में ही उऋण को चुका होता है। आजकल अयोग्य युवक-संन्यासी बहा दिखायी पड़ते हैं। यह प्राचीन नियमों के विरुद्ध है और इससे बहुत व्यवधान उपस्थि हो जाता है।
ब्रह्मचारी
प्रथम आश्रम-ब्रह्मचर्य-अध्ययन और अनुशासन का काल है। विद्यार्थियों को विलासप्रिय नहीं होना चाहिए। वह गुरु के पास रह कर बेदों और विद्याओं क अध्ययन करता है। यह आश्रम उसका परिवीक्षा (probation) काल है। प्राचीन मा में गुरु साधारणतया जंगल में कुटी बना कर रहते थे। ये कुटियाएँ ही गुरुकुत अर्थात् अरण्य विश्वविद्यालय कहलाती थीं। विद्यार्थी भिक्षा-वृत्ति द्वारा भोजन करता था। धनी और निर्धन के बालक साथ-साथ रहते थे। विद्यार्थी गुरु को अपन आध्यात्मिक पिता मानता था और भक्ति, विश्वास और सम्मानपूर्वक उसकी सेवा करता था।
विद्यार्थी का जीवन उपनयन संस्कार (यज्ञोपवीत-संस्कार) से प्रारम्भ होता है। यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है। उसे स्वभाव से सरल और परिश्रमी होन चाहिए। वह प्रातःकाल जल्दी उठ कर स्नान करता है और सन्ध्या तथा गायत्री-जा करता है। वह धर्मग्रन्थों का अध्ययन करता है। वह सरल एवं सन्तुलित भोजन ग्रहा करता है। वह पर्याप्त व्यायाम करता है। वह कठोर भूमि पर सोता है; कोमल सुखदायक बिछौना तथा तकियों का प्रयोग वह नहीं करता। वह अति-नम्र औ आज्ञाकारी होता है; वह गुरुजनों की आज्ञा मानता है और उनका आदर करता है। वा मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने की चेष्टा करता है।
वह निरन्तर गुरु-सेवा में रत रहता है। वह स्त्री, मदिरा, मांस, इत्र, माला स्वादिष्ट भोजन, खट्टे तथा मसालेदार भोज्य पदार्थ, जीव-हिंसा, काम, क्रोध, लोभा नृत्य-गान, संगीत-वादन, जुआ, गपशप, मिथ्यापवाद और असत्य से अपने क बचाता है। वह अकेला सोता है।
विद्यार्थी-जीवन के अन्त में वह अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा दे कर गृहस्थ-जीवन में प्रवेश करने के लिए घर वापस जाने की आज्ञा माँगता है। आज्ञा प्रदान करने से पूर्व गुरु निम्नांकित अन्तिम उपदेश देता है:
"सत्य बोलो। अपने कर्तव्य का पालन करो। वेदाध्ययन से विरत न होओ। सन्तति की परम्परा को विश्रृंखल मत होने दो। गुरु को वांछित दक्षिणा देने के पश्चात् गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर सदैव चलते रहो। अपने कल्याण की उपेक्षा मत करो। अपनी समृद्धि की उपेक्षा मत करो। वेदाध्ययन तथा वेदों के उपदेशों की उपेक्षा मत करो।
"देवों और पितरों के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा मत करो। माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को (गुरु को) देवता मानो और अतिथि को देवता मानो। केवल वही कर्म करो जो दोष-रहित हो। केवल सत्कर्म करो।
"आपको अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आसन आदि दे कर उनकी श्रान्ति दूर करनी चाहिए। उन्हें श्रद्धा, विनम्रता और सहानुभूतिपूर्वक उपहार देना चाहिए। यदि कर्मकाण्ड अथवा आचरण के सम्बन्ध में कोई संशय हो, तो महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लो। यही आज्ञा है, यही शिक्षा है, यही वेदों का रहस्य है। यही दैवी आदेश है। इसका पालन करो। इसी पर मनन करो।"
गृहस्थ
दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम है। जब विद्यार्थी अपना छात्र-जीवन समाप्त करके गृहस्थ-जीवन के उत्तरदायित्व को वहन करने योग्य हो जाता है, तब अपने विवाह के समय वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। समस्त आश्रमों में यह आश्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि यह अन्य समस्त आश्रमों का आधार है। जिस प्रकार समस्त जीवन वायु द्वारा पोषित होते हैं, जिस प्रकार समस्त नदियाँ समुद्र में पहुँच कर विश्राम प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार समस्त आश्रम गृहस्थ-आश्रम में विश्राम पाते हैं। गृहस्थ आर्य-जीवन का हृदय है। प्रत्येक बात उस पर निर्भर रहती है।
हिन्दू के लिए विवाह एक पवित्र संस्कार है। पत्नी उसकी जीवन-संगिनी होती है। वह उसकी अर्धांगिनी होती है। उसके बिना हिन्दू कोई धार्मिक कर्मकाण्ड सम्पन्न नहीं कर सकता। धार्मिक कृत्य करते समय पत्नी पति के बायीं ओर खड़ी होती है। पति-पत्नी राम-सीता को अपना आदर्श मानते हैं।
गृहस्थ को सच्चाई और ईमानदारी से धनोर्पाजन करके उचित ढंग से इसका विभाजन करना चाहिए। उसे अपनी आय का दशवाँ भाग दान में व्यय करना चाहिए। ऐन्द्रिक सुख नीति-सिद्धान्तों की सीमा के भीतर ही भोगने चाहिए। गृहस्थ को माह में केवल एक रात्रि स्त्री-संग का सुख अनुभव करना विहित है।
गृहस्थ को निम्नांकित पाँच महायज्ञ करने चाहिए :
(१) देव-यज्ञ वेदमन्त्रोच्चारण के साथ देवताओं को आहुति देना।
(२) ऋषि-यज्ञ वेदाध्ययन, विद्यार्थियों को वेद पढ़ाना और ऋषियों को आहुति देना ऋषि-यज्ञ के अन्तर्गत
आते हैं।
(३) पितृ-यज्ञ-मृतक आत्माओं को तर्पण देना एवं श्राद्ध अथवा वार्षिक कर्मकाण्ड सम्पन्न करना पितृ-यज्ञ
है।
(४) भूत-यज्ञ-गायों, कौओं तथा पशुओं को भोजन देना भूत-यज्ञ है।
(५) अतिथि-यज्ञ-अतिथियों को भोजन कराना और उनका मान-सम्मान करना अतिथि-यज्ञ है।
आतिथ्य गृहस्थों का प्रधान कर्तव्य है। उसे सर्वप्रथम अपने अतिथियों को, ब्राह्मणों को और सम्बन्धियों को भोजन करा कर तब स्वयं पत्नी सहित भोजन करना चाहिए।
जब गृहस्थ देखे कि उसके पुत्र उसके कर्तव्यों का भार वहन करने में समर्थ हो गये हैं तथा परिवार में उसके पौत्र पौत्रियाँ भी हैं, तब उसे समझना चाहिए कि उसके और उसकी पत्नी के लिए संसार को त्याग कर अध्ययन और चिन्तन में अपना जीवन व्यतीत करने का समय आ गया है।
वानप्रस्थी
इसके पश्चात् वानप्रस्थ-आश्रम की अवस्था है जिसमें गृहस्थ वानप्रस्थी के रूप में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य जिस प्रकार गृहस्थ-जीवन की तैयारी है, उसी प्रकार वानप्रस्थ अन्तिम अवस्था संन्यास की तैयारी है। गृहस्थ-आश्रम के समस्त कर्तव्यों का पालन कर चुकने के पश्चात् मनुष्य को वन में या अन्य कहीं एकान्त-स्थान में जा कर उच्चतर आध्यात्मिक विषयों का चिन्तन-मनन करना चाहिए। अब वह सामाजिक बन्धनों और जीवन के उत्तरदायित्वों से मुक्त है। अब उसके पास धर्मग्रन्थों का अध्ययन करने के लिए प्रचुर अवकाश है। उसकी पत्नी उसके साथ जा सकती है, अन्यथा वह अपने पुत्र के साथ रहने के लिए स्वतन्त्र है।
संन्यासी
अन्तिम अवस्था संन्यास-आश्रम है। संन्यासी होने पर मनुष्य सब-कुछ त्याग देता है-धन-सम्पत्ति, जाति-भेद, कर्मकाण्ड, धर्मानुष्ठान तथा देश, राष्ट्र या धर्म-विशेष के लिए आसक्ति। वह भिक्षा माँग कर निर्वाह करता है। गहन ध्यान की उत्कृष्ट अवस्थाओं में प्रवेश कर लेने के पश्चात् वह अपनी ही आत्मा में आनन्दित हो उठता है। विषय-सुखों से वह विमुख हो जाता है। वह रुचि-अरुचि, इच्छा, अहंभाव, कामुकता, क्रोध, लोभ और अहंकार से मुक्त हो जाता है। उसमें समत्व दृष्टि तथा मानसिक सन्तुलन होता है। वह सबसे प्रेम करता है और ब्रह्मज्ञान वितरित करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक भ्रमण करता है। मान-अपमान, निन्दा-स्तुति और सफलता-असफलता में वह समभाव रखता है। अब वह अति-वर्णाश्रमी हो जाता है अर्थात् वर्णाश्रम से परे हो जाता है। वह सर्वथा मुक्त हो जाता है। वह सामाजिक प्रथाओं और बन्धनों से भी मुक्त है।
ऐसा संन्यासी एक आदर्श पुरुष है। उसने पूर्णता और मुक्ति प्राप्त कर ली है। वह ब्रह्म ही है, जीवन्मुक्त है। इस पृथ्वी पर साक्षात् देवता-स्वरूप ऐसी महान् आत्माओं की जय हो!
आधुनिक परिस्थितियों में आश्रम-धर्म
इस युग में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमों के प्राचीन नियमों का पूरा-पूरा पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना सम्भव नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ गया है; किन्तु उनमें निहित मूल-भावना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इससे आधुनिक जीवन में बहुत सुधार हो सकता है। इन आश्रमों के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए किसी को दूसरे आश्रमों के लिए निर्धारित कर्मों को नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी को गृहस्थों, वानप्रस्थियों अथवा संन्यासियों के लिए विहित कर्म नहीं करने चाहिए। संन्यासी को दोबारा गृहस्थ-जीवन के सुखों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
समाज में शान्ति और व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है, जब प्रत्येक मनुष्य सुचारु रूप से अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करे। वर्णाश्रम-व्यवस्था का उन्मूलन सामाजिक कर्तव्यों को निर्मूल कर देगा, समाज-धर्म को जड़ से उखाड़ देगा। वर्णाश्रम-धर्म का दृढ़तापूर्वक पालन किये बिना कोई भी राष्ट्र कैसे जीवित रहने की आशा कर सकता है!
विद्यार्थियों को पवित्रता और सादगी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थ को आदर्श गृहस्थ का जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे आत्मसंयम, दया, सहिष्णुता, अहिंसा, सत्यता और मिताचार को व्यवहार में लाना चाहिए। जिन्हें वानप्रस्थ एवं संन्यास-आश्रमों का जीवन कठिन प्रतीत होता हो, उन्हें धीरे-धीर सांसारिक जीवन से विरत हो कर निष्काम सेवा, अध्ययन और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।
सर्वोच्च स्थिति
वर्णाश्रम केवल शरीर से ही सम्बन्धित है; शुद्ध, सर्वव्यापक अमर आत्मा मे नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त कर लें तथा दत्तात्रेय की भाँति अति-वर्णाश्रमी बन जायें। दत्तात्रेय के अनुसार-
महदादि जगत्सर्वं न किंचित्प्रतिभाति मे।
ब्रह्मैव केवलं सर्वं कथं वर्णाश्रमस्थितिः ।।
अर्थात् महत् से ले कर नीचे तक अखिल जगत् मुझमें नहीं भासता। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ही है। फिर वर्णाश्रम कहाँ?
ईश्वर करे, आप सबमें वर्णाश्रम और वर्णाश्रम-धर्म का पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो। आप सबमें वैश्व-प्रेम और भ्रातृत्व की भावना विकसित हो ! आत्म-प्रशंसा तथा स्वाग्रह के लिए मनुष्य द्वारा निर्मित समस्त विघटनकारी अवरोध छिन्न-भिन्न हो जायें!
युग-धर्म
सत्ययुग में धार्मिक नियमावली भिन्न थी, त्रेतायुग में उसमें परिवर्तन कर दिया गया। द्वापर का धर्म अन्य युगों से भिन्न था। कलियुग में उन्होंने अन्य रूप धारण किया। धर्म समय-चक्र के साथ परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य परिवर्तित होता रहता है। विभिन्न अनुभवों के कारण उसकी प्रकृति परिवर्तित होती रहती है; इसलिए उसके धर्म का बाह्य रूप भी परिवर्तित होना चाहिए।
सत्ययुग में जो ध्यान-चिन्तन से, त्रेता में जो यज्ञ से और द्वापर में जो विष्णु की उपासना से प्राप्त होता था, वही कलियुग अर्थात् लौहयुग में भगवान् विष्णु के नाम-कीर्तन से प्राप्त किया जा सकता है।
सत्ययुग में मनुष्यों का मन शुद्ध तथा विक्षेप-रहित था। उस युग में न सिनेमा थे, न होटल थे, न नृत्यशालाएँ थीं और न ही विक्षेप उत्पन्न करने वाली अन्य वस्तुएँ थीं। अतः उनके लिए ध्यान-चिन्तन सरल और सहज था। इसलिए सत्ययुग के लोगों के लिए ध्यानयोग को उपयुक्त बताया गया है। त्रेतायुग में यज्ञ-सामग्री सरलता से उपलब्ध होती थी। मनुष्यों की प्रवृत्तियों में सक्रियता थी। अतः उनके लिए अग्रिहोत्र, ज्योतिष्टोम, दर्शपौर्णिमा एवं अन्य यज्ञों को सम्पन्न करना सरल था; इसलिए उस युग में यज्ञ को सनातन धर्म का बाह्य रूप कहा गया। द्वापरयुग में अवतारों की अभिव्यक्ति हुई और लोग सरलता से भगवान् की प्रत्यक्ष उपासना कर सकते थे; इसलिए उस युग में उपासना को साधना का प्रमुख रूप माना गया। कलियुग में विक्षेप के लिए अनुकूल अनेक स्थितियाँ हैं। मनुष्य में ब्रह्मचर्य, इच्छा-शक्ति और विचार और विवेक-शक्ति का अभाव है। यज्ञ करने के लिए सामग्री प्राप्त होना दुर्लभ है। इसलिए हरि-कीर्तन तथा मानवता की निष्काम सेवा साधना के मुख्य स्वरूप बतलाये गये हैं।
उपसंहार
पूर्ण उत्साह से स्वधर्म-पालन करें। अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें। धर्म में निहित समस्त गुणों को विकसित करें। सदाचार के मार्ग से तनिक भी विचलित मत हों। अपने सम्पूर्ण हृदय, मन और आत्मा से धर्म का पालन करें। स्वधर्म-पालन से प्रसन्नता तथा मुक्ति प्राप्त होती हैं तथा आपका क्रम-विकास त्वरित गति से होता है। आपको शीघ्र ही अमरत्व, शाश्वत परमानन्द, परम शान्ति, अखण्ड आनन्द, कैवल्य और पूर्णता प्राप्त होंगे। आपको शाश्वत परमानन्द के राज्य और अनन्त शान्ति के पथ की ओर ले जाने वाले परम ज्योतिरूप धर्म की जय हो!
हिन्दुत्व का शाश्वत धर्म सदा के लिए सुरक्षित रहे ! समस्त हिन्दू सच्चे प्रेम के बन्धन में बंध कर संगठित हों!
चतुर्थ अध्याय
हिन्दू-आचार-नीति
धर्म का चिह्न आचार अथवा सदाचार है। आचार भलाई का चिह्न है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म जीवन को समृद्ध बनाता है। धर्माभ्यास द्वारा मनुष्य इस लोक एवं परलोक में समृद्धि और कीर्ति प्राप्त करता है।
सदाचार सर्वोच्च धर्म है। यह समस्त तप और साधनाओं का आधार है। धर्मपरायणता, सच्चाई, सत्कर्म, शक्ति और समृद्धि-ये सब आचरण से ही उत्पन्न होते हैं।
आचरण और चरित्र
मनुष्य आकांक्षित पदार्थों को पाने की कामना करता है। कामना कार्य-रूप में परिणत होती है। यह आचरण कहलाता है। आचरण है व्यवहार। जो कामनाएँ अभिव्यक्त होती हैं, वे आचरण बन जाती हैं।
मनुष्य की कई प्रकार की इच्छाएँ होती हैं। कभी-कभी इच्छाओं में विरोध उत्पन्न हो जाता है। जो इच्छा विजयी होती है, वह दृढ़ निश्चय (will) कहलाती है। आन्तरिक प्रवृत्ति जो दृढ़ निश्चय को सम्भव बनाती है, वह चरित्र कहलाती है। चरित्र विशिष्ट गुणों का समुच्चय है जिससे व्यक्तिकता का निर्माण होता है।
मनुष्य के चरित्र की परीक्षा करने के लिए उसका बाह्य व्यवहार सदैव एक विश्वस्त पथ-प्रदर्शक सिद्ध नहीं होता है।
आचार-नीति अर्थात् आचरण-विज्ञान
नैतिकता (morality) अथवा आचार-नीति (ethics) आचरण का विज्ञान है। चरित्र में अच्छे-बुरे का अध्ययन आचार-नीति है। आचार-नीति का विज्ञान मनुष्यों को एक-दूसरे के प्रति एवं अन्य जीवों के प्रति व्यवहार करने का ढंग बताता है। इसमें वे विधिसंगत सिद्धान्त निहित हैं जिनके अनुसार मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए। आचार-नीति है सदाचार।
नैतिकता कई प्रकार की होती है-मानवीय नैतिकता, पारिवारिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, राष्ट्रीय नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता। डाक्टर व्यावसायिक नैतिकता का ध्यान रखता है। उसे अपने रोगियों के गुप्त रहस्यों को दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि किसी महामारी को रोकने के लिए वह सारे वारणिक उपाय करे और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई की ओर पूरा-पूरा ध्यान दे।
आचार-नीति एक सापेक्ष विज्ञान है। सम्भव है जो बात एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो, वह दूसरे के लिए अच्छी न हो। जो बात किसी विशिष्ट काल में और स्थान पर अच्छी हो, वह किसी अन्य काल तथा अन्य स्थान में अच्छी नहीं भी हो सकती है। नीतिशास्त्र स्वयं मनुष्य और उसके चतुर्दिक् के वातावरण के लिए प्रासंगिक है।
आचार-नीति, आध्यात्मिकता और धर्म
बिना आचार-नीति के आप आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति नहीं कर सकते। आचार-नीति योग का आधार है। यह वेदान्त की आधारशिला है। यह वह दृढ़ स्तम्भ है जिस पर भक्तियोग का भवन टिका हुआ है। यह भगवत्साक्षात्कार का प्रवेश-द्वार है।
आचार-नीति की पूर्णता के बिना आध्यात्मिक उन्नति अथवा साक्षात्कार सम्भव नहीं है। योग के विद्यार्थी अथवा साधक में आचार-नीति विषयक दृढ़ता होनी चाहिए। उसे विचार, वाणी तथा कर्म से शुद्ध और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। उसका आचरण उत्कृष्ट होना चाहिए। उसे किसी भी जीव को विचार, वाणी अथवा कार्य से नहीं सताना चाहिए। उसे सम्यक् विचार, सम्यक् वाणी और सम्यक् कर्म का पूर्णरूपेण अभ्यास करना चाहिए।
प्रत्येक धर्म की अपनी आचार-नीति होती है। ईसामसीह के शैलोपदेश (Sermon on the Mount) तथा दशादेश (Ten Commandments) में मनुष्य के उत्थान के लिए नैतिक शिक्षाएँ हैं। भगवान् बुद्ध का अष्टांग मार्ग नीतिशास्त्र का सारतत्त्व है। पतंजलि महर्षि के यम तथा नियम उत्कृष्ट नीतिशास्त्र के अंग हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति और पाराशरस्मृति में भी मानव के लिए आचार-संहिता प्रस्तुत की गयी है। गीता में वर्णित तीन प्रकार के तप आचार-नीति का ही एक गहन स्वरूप हैं।
आचार-नीति का अभ्यास करने के लाभ
नैतिकता धर्म का प्रवेश-द्वार है। जो नीतिसंगत अथवा सद्गुणों से पूर्ण जीवन व्यतीत करता है, वह निर्वाण, पूर्णता अथवा मोक्ष प्राप्त करता है।
आचार-नीति के अभ्यास से आपको अपने पड़ोसियों, मित्रों, कुटुम्बिों, संगी-साथियों तथा अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन व्यतीत करने में सहायता मिलेगी। इसके अभ्यास से आपको स्थायी सुख और मोक्ष प्राप्त होगा। इससे आपका हृदय पवित्र तथा अन्तःकरण निर्मल बनेगा। नीतिशास्र के सिद्धान्तों का पूर्णतया पालन करने वाला नैतिक मनुष्य धर्म अथवा न्याय के मार्ग से किंचित् भी च्युत न होगा। युधिष्ठिर ने आचार-नीति के अभ्यास के कारण शास्वत प्रतिष्ठा प्राप्त की। वह धर्म की प्रतिमूर्ति थे; इसलिए वह अब तक हमारे हृदयों में प्रतिष्ठित हैं।
सदाचरण भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का मूल है। आचरण से ख्याति में वृद्धि होती है। सदाचरण आयु को बढ़ाता, समस्त विपदाओं एवं बुराइयों को नह करता और शाश्वत सुख प्रदान करता है। सदाचरण ही गुणों को जन्म देता है। अतः सदाचरण विकसित करें।
हिन्दू-धर्म में आचार-नीति की संहिताएँ
हिन्दू आचार-नीति सर्वोपरि है। हिन्दू धर्म में नैतिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। यम तथा नियम योग और वेदान्त की नींव हैं। अविकसित मनुष्य स्वयं अपने लिए नहीं सोच सकते; इसलिए मनु और याज्ञवल्क्य जैसे महान् सन्तों और द्रष्टाओं ने आचरण के नियम बनाये हैं।
गीता में भगवान् कृष्ण कहते हैं- "कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय करने में शास्त्रों को अपना प्रमाण मानें। आपको शास्त्र-विधि से नियत किये गये कर्मों को ही करना चाहिए" (१६/२४)। याज्ञवल्क्य, मनु एवं ऋषियों द्वारा रचित स्मृतियों में स्पाह रूप से सदाचार के नियम निर्धारित किये हैं। आपमें शास्त्रोक्त नैतिक सिद्धान्तों और नियमों पर विचार करने हेतु क्षमता तथा समय का अभाव है; अतः आपको सन्त-महात्माओं से ही नीति-सम्बन्धी तत्त्व ग्रहण करके उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए।
हिन्दू-आचार-नीति के मौलिक सिद्धान्त
हिन्दुओं की आचार-नीति सूक्ष्म, भव्य और गहन है। समस्त धमों ने आचार-नीति-सम्बन्धी विचारों की शिक्षा दी है, यथा- 'हिंसा मत करो, दूसरों को चोट मत पहुँचाओ, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो।' परन्तु उन्होंने कारण नहीं बताया है। हिन्दू-आचार-नीति का आधार है- "सर्वव्यापक आत्मा एक है। वह समस्त जीवों का अन्तरात्मा है। वह सामान्य पवित्र चेतना है। यदि आप अपने पड़ोसी को या किसी अन्य जीव को क्षति पहुँचाते हैं, तो आप अपने को ही क्षति पहुँचाते हैं; क्योंकि अखिल विश्व आपके अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं है।" यह हिन्दू-आचार-नीति है। यह मूलभूत तात्त्विक सत्य है जो समस्त हिन्दू-आचार-नीति-सिद्धान्तों का आधार है।
आत्मा एक है। समस्त जीवों में एक ही प्राण स्पन्दित होता है। पुरुष, पक्षी और मानव-जाति में जीवन समान है। अस्तित्व समान है। यह उपनिषदों अथवा श्रुतियों की सुस्पष्ट घोषणा है। धर्म का यह मौलिक सत्य आचार-नीति अथवा नैतिकता अथवा सम्यक् आचरण के विज्ञान का आधार है। वेदान्त नैतिकता का आधार है।
प्रथम बात जो धर्म सिखाता है, वह है सब आत्माओं में निहित एकता। उपनिषदों का कथन है- "तेरा पड़ोसी वस्तुतः तू स्वयं है-जो तुझे उससे पृथक् करता है, वह मात्र एक भ्रम है।" एक आत्मा सब जीवों में निवास करती है। सार्वभौमिक प्रेम इस एकता की अभिव्यक्ति है। आत्मैक्य सार्वभौम भ्रातृत्व का आधार है। समस्त मानवीय सम्बन्ध इसी एकता पर टिके हुए हैं। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा- "प्रिय! देखो, केवल पति-प्रेम के कारण पति प्रिय नहीं है, आत्मा के प्रति प्रेम के कारण पति प्रिय होता है।" इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, धन-सम्पत्ति, मित्र, संसार और स्वयं देवता भी अपनी आत्मा के कारण प्रिय हैं। सब इसलिए प्रिय हैं; क्योंकि सबमें एक ही आत्मा विद्यमान है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुँचाते हैं, तो आप अपने को ही क्षति पहुँचाते हैं; यदि आप किसी की सहायता करते हैं, तो आप अपनी ही सहायता करते हैं। सब प्राणियों में एक ही प्राण तथा एक ही सामान्य चेतना है। यही सम्यक् आचरण की नींव है। यही आचार-नीति का आधार है।
उपासना के रूप सेवा
मात्र प्रकार समाज-सेवा समझता उसमें भाव नहीं कि समस्त विश्व परमात्मा का प्रकटीकरण वह परमात्मा ही सेवा कर रहा है। उसमें यह भी नहीं परमात्मा उसके उपकरणों (इन्द्रियों) के माध्यम से कार्य कर रहा और प्रत्येक परमात्मा को अर्पित भेंट एक यौगिक क्रिया है।
भारतवर्ष में व्यक्तियों को आमन्त्रित करने ५०० व्यक्तियों भोजन तैयार किया जाता हिन्दुओं लिए खिलाना परमात्मा उपासना है। यह अतिथि-यज्ञ है। हिन्दू प्रत्येक प्राणी को भगवान् है।
हिन्दू बड़े उदार, उदात्त, विशाल-हृदय, परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण, दयावान् सत्कारशील होते किसी देख अपने घर जायेंगे उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, मानो वह अतिथि हो। पहले उसे भोजन करवा कर वे भोजन करेंगे। संसार में कहीं ऐसा व्यवहार देखने-सुनने को नहीं मिलेगा। अन्य देशों भोजन का एक ग्रास भी बिना सकता।
हिन्दुओं विश्वास कि एक सन्त-महात्मा को अखिल विश्व को भोजन दे क्योंकि ज्ञान हो है कि साक्षात्कार प्राप्त सन्त ब्रह्म से एकाकार होता वह सारी सृष्टि से एकरूप हिन्दू-नीति-शास्त्र वेदान्त उत्कृष्ट दर्शन पर आधारित दर्शन जीवन एकत्व और चेतना सिद्धान्त को मानता नैतिकता एवं परोपकार इसी एकत्व अभिव्यक्तियाँ हिन्दू स्वयं भोजन से कौओं, कुत्तों, गायों और मछलियों भोजन देता है। सब रूपों में अन्तर्निहित एकमेव आत्मा ही महचानने प्रयास करता है। वह है कि दूसरों प्रेम करना को प्रेम है को कष्ट पहुँचाना स्वयं कष्ट पहुँचाना वैश्व-प्रेम के अभ्यास द्वारा अनुभव सारे के हैं, सारे पाँव उसी हैं और अखिल विश्व उसका आवास है (वसुधैव कुटुम्बकम्) धीरे-धीरे वह ब्रह्माण्ड आत्मा से एकाकार हो जाता है और परमात्मा से भी। हिन्दू-आचार-नीति धीरे-धी आत्मसाक्षात्कार की ओर प्रवृत्त करती है। आचार-नीति योग का एक साधन है।
आचार-नीति के संवर्धन अथवा शोधन की प्रक्रिया
समस्त नैतिक अनुशासनों का मूल मानसिक शोधन है। यह शोधन समस्त दुष्कर्मों से बचते हुए सद्गुणों के सक्रिय अभ्यास द्वारा ही सम्भव हो सकता है। हर समय भलाई करें। अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य पाप से बचने, सद्गुणों को अपनाने और आत्म-शोधन की तीन प्रक्रियाओं के प्रतीक हैं।
मनुष्य के अहंकार से ही सारी बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। अहंकार अपने को आकांक्षा, इच्छा और लोभ के रूपों में व्यक्त करता है। इसके प्रभाव से मनुष्य घृणा, प्रेम, चाटुकारिता, अभिमान, अनैतिकता, मिथ्याचार, कूटनीति और भ्रान्ति में रस लेने लगता है।
देहाभिमान से उत्पन्न अहंकार का उन्मूलन करने हेतु शरीर की बुराइयों तथा नश्वरता पर सतत विचार करें। बुराई समझ कर उनका बहिष्कार करें और मानसिक रूप से उनसे ऊपर उठ जायें। जो वांछनीय है, उन्नयनकारी और दिव्य है, उसी का चिन्तन-मनन करें।
अनुचित कृत्य (विवेक की उपेक्षा करके किया गया अविचारपूर्ण कर्म) से ही समस्त प्रकार की विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। विपत्तियों से मुक्ति पाने हेतु सदाचार का पालन करना चाहिए। अपने विचार, वाणी, कर्म आन्तरिक उद्देश्य तथा सामान्य आचरण में सत्य एवं पवित्रता का पालन दृढ़तापूर्वक करें। मनुष्य और वस्तुओं के प्रति कोई धारणा निर्मित करते समय तथा दूसरों के साथ अपने व्यवहार में स्नेह, सहनशीलता तथा उदारता का परिचय दें।
हर क्षेत्र में मनुष्य को इन सद्गुणों का अभ्यास करने तथा इनको व्यक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पिता-पुत्र, बड़े-छोटे, शिक्षक-विद्यार्थी, मित्र-मित्र, गुरु-शिष्य, नेता-अनुयायी, प्रजा-प्रशासक और राष्ट्र-राष्ट्र के पारस्परिक सम्बन्धों में हमें इस आदर्श को चरितार्थ करना चाहिए।
आपको सद्गुण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इस बात का निश्चय कर लें कि आप धर्म से किंचिन्मात्र कदापि विचलित नहीं होंगे। आपको अपने मन को सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित करना होगा और अपनी इच्छा-शक्ति को विकसित करना और बलवती बनाना होगा। इसी कारण यम, नियम और षट्सम्पत् पर बहुत बल दिया गया है। नित्य-प्रति के जीवन में किये गये आत्मत्याग एवं बलिदान के संकल्पित कर्मों द्वारा मन और इच्छा-शक्ति को प्रयोग में लाना एवं उन्हें अनुशासित बनाना चाहिए। इस प्रकार आचार-नीति के संवर्धन के लिए दो बातें आवश्यक हैं- निक जागरूकता और सम्यक् अभ्यास। आचार-नीति के संवर्धन में संवेदनशील सदसद्विवेक तथा भलाई एवं श्रेष्ठता के प्रति सुनिश्चित श्रद्धा का महत्वपूर्ण सवार होता है।
औचित्य तथा अनौचित्य का दर्शन
प्रत्येक व्यक्ति कहता है-"यह उचित है, वह अनुचित है, तुम्हारा कथर (अथवा व्यवहार) उचित है, उसका कथन (अथवा व्यवहार) अनुचित है"; परन वह यह ठीक-ठीक नहीं बतला सकता है कि 'उचित' तथा 'अनुचित' से उसका स्वा अभिप्राय है।
वह मापदण्ड क्या है जिससे आप किसी कार्य के उचित-अनुचित अथवा अच्छे-बुरे होने का निर्णय लेते हैं? उचित-अनुचित और भला-बुरा सापेक्ष शब्द है। उचित तथा अनुचित नैतिक स्तर से वैधिक पक्ष को और भलाई तथा बुराई इसके परिणामात्मक पक्ष को व्यक्त करते हैं। आपको अपना आचरण इस स्तर के अनुकूल बनाना होगा। जो किसी नियम के अनुसार होगा, वह उचित है। जो उपलब्ध करने योग्य है, वह अच्छा है। धर्म हमें नैतिक विज्ञान के आधार के लिए अन्तिम रूप में मान्य सामग्री प्रदान करता है।
औचित्य-अनौचित्य की सापेक्षता
सही और गलत तथा धर्म और अधर्म सापेक्ष शब्द हैं। इन नियमों को यथातथ्य परिभाषित करना बहुत कठिन है। कभी-कभी सन्त जन भी यह निर्णय करने में सम्भ्रमित हो जाते हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों में क्या उचित और क्या अनुचित है। इसीलिए भगवान् कृष्ण ने भी गीता में कहा है- "क्या कर्म और क्या अकर्म है, इस विषय में बुद्धिमान् पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं; इसलिए मैं तुझे उस कर्म के विषय में बतलाऊँगा जिसे जान कर तू अशुभ से मुक्त हो जायेगा। तुझे कर्म, अकर्म और निषिद्ध कमाँ का स्वरूप अवश्य जानना चाहिए। कर्म की गति गहन है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान् है। वह समस्तः कर्म करते हुए भी योगयुक्त है" (४/१६, १७ और १८)।
उचित-अनुचित के उदाहरण
उचित तथा अनुचित सदा चतुर्दिक् परिस्थितियों के अनुसार सापेक्ष होते हैं। एक स्थिति में जो उचित है, दूसरी स्थिति में वही अनुचित हो जाता है। उचित और अनुचित समय, विशेष परिस्थितियों, वर्ण और आश्रम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। नैतिकता एक परिवर्तनशील और सापेक्ष शब्द है। जो व्यक्ति किसी कुख्यात महिला के घर छह महीने में एक बार ही जाता है, उसकी अपेक्षा वह विषयी पुरुष अधिक अनैतिक है जो अपनी वासनापूर्ति के लिए अपनी विधिवत् विवाहित पत्नी को बार-बार उत्पीड़ित करता रहता है। अनैतिक विचारों में निरन्तर लीन रहने वाला मनुष्य सर्वाधिक अनैतिक है। दोनों में यह सूक्ष्म भेद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। क्षत्रिय राजा के लिए शत्रु को मारना उचित है। ब्राह्मण या संन्यासी के लिए खतरे के समय अपनी रक्षा करने हेतु भी किसी को मारना उचित नहीं। उन्हें कठोर सहिष्णुता और क्षमाशीलता का अभ्यास करना चाहिए। किसी महात्मा या गुरु पर यदि किसी अन्यायी अधिकारी द्वारा अन्यायपूर्ण अभियोग लगाया गया है, तो उसका जीवन बचाने के लिए झूठ बोलना ठीक है। इस विशिष्ट परिस्थिति में असत्य सत्य बन गया है। परन्तु ऐसा सत्य जिससे बहुतों को हानि पहुँचे, असत्य ही है। पथिकों की नित्य हत्या करने वाले डाकू की हत्या अहिंसा ही है। विशेष परिस्थितियों में हिंसा अहिंसा बन जाती है।
निवृत्ति-मार्ग पर चलने वाले संन्यासी या तपस्वी को क्षमा शोभा देती है; परन्तु शासक को शोभा नहीं देती। अपने को हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति को शासक क्षमा कर सकता है; परन्तु जनता को अत्यधिक हानि पहुँचाने वाले को नहीं।
संकटपूर्ण परिस्थितियों के लिए कतिपय विशिष्ट धर्म होते हैं, जिन्हें आपद्-धर्म कहते हैं। जब भयंकर अकाल पड़ा तो ऋषि विश्वामित्र ने एक चाण्डाल से मांस ले कर देवयज्ञ में चढ़ाया। सन्त उशस्ति ने एक महावत से उच्छिष्ट अन्न ले कर खा लिया था, क्योंकि वह बहुत भूखे थे और कहीं से भोजन पाने में समर्थ नहीं थे।
औचित्य तथा अनौचित्य के सूचक
वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कणाद (इस दर्शन के) प्रथम सूत्र में कहते हैं- "जो तुम्हारे ऊर्ध्वगमन में सहायक बन कर तुम्हें परमात्मा के समीप ले जाये, वह उचित है। जो तुम्हारे अधोगमन का कारण बने और तुम्हें परमात्मा से दूर ले जाये, वह अनुचित है। जो धर्मग्रन्थों में उल्लिखित आदेशों के सर्वथा अनुकूल है, वह उचित है और जो उन आदेशों के प्रतिकूल है, वह अनुचित है।" यह उचित-अनुचित का परिभाषित करने का एक ढंग है। ईश्वरेच्छा के अनुकूल कार्य करना उचित तथा उसके प्रतिकूल कार्य करना अनुचित है।
एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह जानना कठिन है कि किन्हीं विशिष्ट कायों से कौन-सी ईश्वरीय इच्छा निहित है। इसीलिए मनीषी सन्तों ने यह घोषणा की है कि सम्बन्ध में लोगों को शास्त्रों, विद्वान् पण्डितों और आत्मज्ञानी पुरुषों द्वारा मान्य विचारों को स्वीकार करना चाहिए। जिसने वर्षों पर्यन्त निष्काम कर्मयोग का अभ्यास किया हो और दीर्घकाल तक ईश्वरोपासना की हो, ऐसा पवित्र पुरुष जब कुछ विष्टि कार्य करना चाहता है, तो उसे सहज ही ईश्वरीय इच्छा का पता लग जाता है। वह उस (इच्छा) की आन्तरिक, तीव्र तथा मौन वाणी सुन सकता है। साधारण मनुष्यों को यह दिव्य वाणी सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वे विकृत मन की वाणी को ईश्वरीय वाणी समझने की भूल कर सकते हैं। उनका निम्न वृत्तिक मन उन्हें भ्रमित कर देगा।
स्वार्थभाव बुद्धि को आच्छादित कर देता है। इसलिए यदि मनुष्य में लेशमात्र भी स्वार्थभाव है, तो वह उचित तथा अनुचित में भेद नहीं कर सकता। उसके लिए अति पवित्र, सूक्ष्म और तीव्र बुद्धि की आवश्यकता है। गीता में सात्त्विक, राजसी और तामसी बुद्धि का वर्णन इस प्रकार किया गया है-
"हे पार्थ! जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति-मार्ग को, कर्तव्य-अकर्तव्य को, भय-अभय को तथा बन्धन-मोक्ष को तत्त्व से जानती है, वह बुद्धि सात्त्विक है। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म-अधर्म तथा कर्तव्य-अकर्तव्य को ठीक-ठीक नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा सम्पूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है" (१८/३०, ३१ और ३२)।
सदाचार के पथ पर अग्रगामी साधकों की सहायता के लिए विद्वानों द्वारा अनेक परिभाषाएँ दी गयी हैं। बाइबिल में कहा गया है- "दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें, जिस व्यवहार की आप अपने लिए उनसे आशा करते हैं।" यह बहुत सुन्दर नीति-वचन है। इसमें सदाचार का सम्पूर्ण सार निहित है। यदि कोई व्यक्ति सावधानी से इसका आचरण करे, तो वह कोई अनुचित कार्य नहीं करेगा। जो आपके लिए हितकर नहीं है, वैसा दूसरों के साथ भी न करें, जिससे दूसरों की भलाई न हो अथवा जो दूसरे को चोट पहुँचाये और जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। वही कर्म करें जिससे दूसरों की भलाई हो तथा जो प्रशंसनीय हो। वैसा ही व्यवहार करें जिसकी आप अपने लिए दूसरों से आशा करते हैं। यही धर्म का रहस्य है। यही कर्मयोग का सार है। सम्यक् (औचित्यपूर्ण) आचरण की यह संक्षिप्त विवेचना है। ऐसे आचरण से आपको शाश्वत आनन्द की प्राप्ति होगी।
"अहिंसा परम धर्म है।" मन, वाणी तथा कर्म से किसी को चोट न पहुँचाना सर्वगुणों में उत्कृष्ट गुण है। मन, वाणी और कर्म से अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी अनुचित कर्म नहीं कर सकता। इसी कारण महर्षि पतंजलि ने अपने राजयोगदर्शन में अहिंसा को बहुत महत्त्व दिया है। यम के अभ्यास में अहिंसा का प्रथम स्थान है। दूसरों को सुख पहुँचाना उचित है; उन्हें कष्ट और पीड़ा पहुँचाना अनुचित है। दैनिक व्यवहार में इस सिद्धान्त का पालन करता हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर अपना क्रमविकास कर सकता है। ऐसा कोई कर्म न करें जिसके फलस्वरूप आपको भयभीत अथवा लज्जित होना पड़े। इस सिद्धान्त का पालन करने पर आप सर्वथा सुरक्षित रहेंगे। आपके विवेक तथा बुद्धि को जो भी सिद्धान्त अनुकूल प्रतीत हो, मनोयोग और आस्थापूर्वक उसी का पालन करते रहें। आप उन्नत हो कर परमानन्द-धाम को प्राप्त होंगे।
जो कार्य मन को उन्नत करे तथा शान्ति एवं सुख प्रदान करे, वह उचित है; जो कार्य मन में विषाद, पीड़ा और व्याकुलता को उत्पन्न करे, वह अनुचित है। उचित-अनुचित के परीक्षण का यह एक सरल उपाय है।
आध्यात्मिक क्रमविकास में सहायक कर्म उचित है और इसमें बाधा डालने वाला कर्म अनुचित है। आत्मैक्य की ओर अग्रसर करने वाला कर्म उचित है और विभिन्न जीवात्माओं में पार्थक्य की भावना उत्पन्न करने वाला कर्म अनुचित है। धर्मशास्त्रों के आदेशों के अनुकूल कर्म उचित है और उनके प्रतिकूल कर्म अनुचित है। ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल कर्म उचित है और ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल कर्म अनुचित है। परोपकार, सेवा और सहायता करना तथा दूसरों को सुख देना उचित है। दूसरी ओर, दूसरों को कष्ट देना और चोट पहुँचाना अनुचित है। किसी जीव को क्षति न पहुँचाने के भाव से किया गया कर्म निश्चित ही नैतिकता है। नैतिक आदेश जीवों को सब प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त रखने के लिए बनाये गये हैं।
दानशीलता उचित क्यों है? क्योंकि वह 'दान करो' के सिद्धान्त के अनुरूप है। चोरी अनुचित क्यों है? क्योंकि यह अस्तेय के सिद्धान्त के विरोध में है। दुःख और कठिनाई में पड़े किसी व्यक्ति की सहायता करना क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे आपका चरित्र परिष्कृत होगा। इसे आपके हृदय में दयाभाव जाग्रत होगा। सदगुणों के अभ्यास द्वारा आपको भगवत्साक्षात्कार करने में सहायता मिलेगी। जीव-हिंसा में क्या बुराई है? क्योंकि इसका लक्ष्य अशोभनीय है। इससे आपका चरित्र भ्रष्ट हो जायेगा। इससे आप पशुओं के समान क्रूर बन जायेंगे।
यौगिक उद्यानकर्म
अनुचित कर्मों द्वारा आप अपने चरित्र को दूषित करते हैं। अच्छे कर्मों द्वारा आप श्रेष्ठ चरित्र का विकास करते हैं। चरित्रहीन व्यक्ति पाशविकता के स्तर पर उतर आता है। चरित्रवान् व्यक्ति सर्वत्र सम्मान्य, श्रद्धेय तथा पूज्य माना जाता है। सर्वत्र उस पर विश्वास किया जाता है। अतः यौवनकाल में ही सच्चरित्र का विकास करें। हृदय-रूपी उद्यान में दोषों को निराना और सद्गुणों का कर्षण करना सीखें। अवगुण तथा बुरी आदतें झाड़ियाँ हैं। सद्गुण अमूल्य फल-फूल हैं। प्रतिपक्ष-भावना की यौगिक विधि सीखें। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार एवं स्वार्थपरता के विपरीत गुण पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य, क्षमाशीलता, उदारता, नम्रता और निःस्वार्थता हैं। कुशल यौगिक माली बनें। हृदय-रूपी उद्यान में सुन्दर पुष्पों का रोपण करें और हृदय उद्यान के मध्य भगवान् की प्रतिष्ठा करके उन पर ध्यान करें। आप शाश्वत आनन्द और अनश्वरता का उपभोग करेंगे।
उपसंहार
आपको आचरण के नियमों का पालन करना चाहिए। विधिकर्ताओं ने आपकी अपनी उन्नति तथा आध्यात्मिक क्रमविकास के लिए ये नियम बनाये हैं। विधिकर्ता महान् सन्त थे। उन्हें प्रत्यक्ष भगवत्साक्षात्कार हुआ था।
सदाचार का पालन करते रहना निःसन्देह कठिन है। जो ऐसा करता है, उसे उपहास, वैमनस्य और अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। अतएव सहिष्णुता, दैन्य-भाव, मौन, सहनशीलता और क्षमा-भाव-इन गुणों का विकास करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। किसी भी मूल्य पर सदाचार की मर्यादा बनाये रखें। इसके लिए किसी भी प्रकार का मिथ्यापवाद सहन करने के लिए तैयार रहें। बुराई के बदले भलाई करें।
जीवन संकट में हो, तो नैतिकता का मार्ग न छोड़ें। भौतिक लाभ प्राप्त करने के लोभ में सदाचार का त्याग न करें। जब कभी भी किसी प्रकार भ्रम उत्पन्न हो जाये, तब शास्त्रों तथा सन्त जनों से शिक्षा लें। चरित्र-निर्माण करें। विकसित हों। अपना आदर्श सदा अपने समक्ष रखें। सदाचार का सदैव पालन करें। आप शीघ्र ही शाश्वत आनन्द एवं अमृतत्व प्राप्त करेंगे।
पंचम अध्याय
हिन्दू-सिद्धान्त
कर्म का सिद्धान्त
कर्म क्या है?
कर्म का अर्थ कार्य (क्रिया) ही नहीं, प्रत्युत् उसका परिणाम (फल) भी है। किसी कर्म का फल वस्तुतः कर्म से भिन्न नहीं है। यह (फल) कर्म का ही एक भाग है। इसे उससे (कर्म से) पृथक् नहीं किया जा सकता। श्वास-प्रश्वास, चिन्तन, वार्तालाप, दर्शन, श्रवण, भोजन करना आदि कर्म हैं। चिन्तन मानसिक कर्म है। कर्म हमारे वर्तमान जीवन के तथा इससे पूर्व-जन्मों के कार्यों का योग है।
कोई भी कार्य या विचार, जिसका परिणाम निकलता है, कर्म कहलाता है। कर्म के सिद्धान्त का अर्थ है-कार्य-कारण-सिद्धान्त। जहाँ कारण है, वहाँ कार्य अवश्य फलित होगा। बीज वृक्ष का कारण है। वृक्ष कार्य-रूप है। जब वृक्ष बीज उत्पन्न करता है, तब वह बीज का कारण बन जाता है।
कर्म किस प्रकार बनते हैं?
'मानव-प्रकृति त्रिविध है-इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इन तीनों से कर्म बनता है।
कर्म की पृष्ठभूमि में इच्छा और विचार विद्यमान रहते हैं। किसी वस्तु के लिए इच्छा मन में उत्पन्न होती है। तब आप सोचते हैं कि उसे कैसे प्राप्त करें। फिर आप उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इच्छा, विचार और कर्म सदैव साथ रहते हैं। यही मानो कर्म-रूपी रज्जु के तीन सूत्र हैं।
इच्छा कर्म को उत्पन्न करती है। आप आकांक्षित पदार्थों को प्राप्त करने हेतु कर्म तथा प्रयास करते हैं। कर्म के फलस्वरूप दुःख-सुख की उत्पत्ति होती है। अपने कर्मों का फल पाने के लिए आपको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। यही कर्म का सिद्धान्त है।
कर्म-सिद्धान्त की प्रक्रिया
हिन्दू-धर्म में ही नहीं, प्रत्युत् बौद्ध और जैन धर्मों में भी कर्म का सिद्धान्त मौलिक सिद्धान्तों में से एक है। मनुष्य जैसा बीज बोता है, वैसी फसल काटता है। यह कर्म का सिद्धान्त है। यदि आप बुरे कर्म करेंगे, तो उसका बुरा फल आएको भोगना पड़ेगा। यदि अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अवश्य सुख प्राप्त होगा। पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कमों को अपने फल उत्पन्न करने से रोक सके। प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म मानो शाश्वत ईश्वरीय न्याय की तराजू पर तोले जाते हैं। कर्म का सिद्धान्त अटल है।
इस सृष्टि में अनायास ही और अव्यवस्थित ढंग से घटनाएँ घटित नहीं होतीं। वे नियमित रूप से उत्तरोत्तर घटित होती हैं। वे एक नियमित क्रम से एक-दूसरे का अनुगमन करती हैं। जो-कुछ आपके द्वारा अब हो रहा है और जो भविष्य में घटित होगा, उनके बीच एक निश्चित सम्बन्ध है।
प्रत्येक कर्म का त्रिविध परिणाम होता है। वह आपको समुचित पुरस्कार या फल देता है। वह आपके चरित्र को भी प्रभावित करता है और आपके मानस पर अपनी छाप छोड़ देता है। यह छाप उस कृत्य को पुनः करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। बाहरी या भीतरी प्रेरणा के कारण मानसिक छाप मन में एक विचार तरंग का रूप धारण कर लेगी। प्रत्येक कर्म का प्रभाव संसार पर भी पड़ता है।
जैसी करनी, वैसी भरनी
पृथ्वी में छोटा-सा बीज बो देने से छोटा-सा अंकुर निकलता है। फिर अंकुर से पत्तियाँ निकलती हैं। तब उसमें फूल और फल लगते हैं। फल में दोबारा बीज आते हैं। आम के बीज से आम का पेड़ उत्पन्न होता है। यदि आप धान बोयेंगे तो गेहूँ की फसल की आशा नहीं कर सकते। जिस प्रकार का बीज होगा, उससे उसी प्रकार का पौधा उत्पन्न होगा। स्त्री के गर्भ से मानव ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार घोड़े से घोड़ा और श्वान से श्वान ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यदि आप कुकर्म के बीज बोयेंगे, तो उनसे दुःख और कष्ट की फसल ही पैदा होगी। यदि आप सत्कर्मों का बीज बोते हैं, तो आप सुख की फसल काटेंगे। यही कर्म का सिद्धान्त है।
जो-कुछ आप अपने कर्मों द्वारा बोते हैं, वह आपको वापस मिल जाता है। यदि आप सेवा, दान और दया के कार्यों द्वारा दूसरों को सुखी बनाते हैं तो आप सुख का बीज बोते हैं। उससे आपको सुख-रूपी फल प्राप्त होगा। यदि आप कठोर शब्दों, अपमान, दुर्व्यवहार, क्रूर कृत्यों और अत्याचार द्वारा दूसरों को दुःख देते हैं, तो आप. दुःख का बीज बोते हैं। इस बीज से आपको पीड़ा, कष्ट, विपत्ति और दुःख का फल प्राप्त होगा। यह कर्म का अपरिवर्त्य सिद्धान्त है।
भूतकाल में किये हुए आपके कर्म वर्तमान परिस्थिति के लिए उत्तरदायी हैं और वर्तमान कर्म आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। विश्व में अव्यवस्था या स्वेच्छाचार की तरह की कोई स्थिति नहीं है। आप अपने अच्छे कर्मों से अच्छे बनते हैं और बुरे कर्मों से बुरे।
यदि आप बुरे विचारों को प्रश्रय देते हैं, तो इसका कुपरिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तब आप कठिनाई में पड़ेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों से घिर जायेंगे। तब आप अपने वातावरण और परिस्थितियों को दोष देंगे। इस कर्म-सिद्धान्त को भली प्रकार समझ कर बुद्धिमत्ता से रहें। श्रेष्ठ विचारों को स्वीकार करें। आप सदा सुखी रहेंगे।
कर्म, आदतें, चरित्र और भाग्य
विचार आपके भाग्य के निर्माता हैं। यदि आप श्रेष्ठ विचार रखेंगे, तो श्रेष्ठ चरित्र विकसित होगा; कुविचार रखेंगे, तो अधम चरित्र विकसित होगा। यह प्रकृति का अपरिहार्य नियम है। इसलिए आप उदात्त विचारों को पोषित करके सोच-समझ कर अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। विचार स्थूल रूप धारण करके कर्म बन जाता है। यदि आप मन को अच्छे तथा उन्नयनकारी विचारों पर ही टिका सकें, तब स्वभावतः आप अच्छे और प्रशंसनीय कार्य करेंगे।
आपका आचरण आपके चरित्र को प्रकट करता है। आचरण से आपका चरित्र बनता भी है। सदाचार को पोषित (विकसित) करने हेतु अनुशासन और अविरत सतर्कता की आवश्यकता है। आपको अपने प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म के प्रति जाग्रत रहना होगा। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय आपको अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। सदाशय रखते हुए भी पूर्व-संस्कारों, प्रवृत्तियों और मनोवेगों के वशीभूत हो कर आप विचलित हो सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी सम्यक् व्यवहार करना नहीं जानते। सद्व्यवहार से यह प्रकट होता है कि आपका मन परिष्कृत (परिमार्जित) और संयमित है और आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सचमुच श्रेष्ठ तथा आध्यात्मिक है। जप, प्राणायाम और मौनव्रत के अभ्यास से मनोवेगों आदि को नियन्त्रित करने में सहायता मिलेगी।
कर्म के बीज बो कर स्वभाव की फसल काटी जाती है। स्वभाव बो कर चरित्र की फसल प्राप्त होती है। चरित्र का वपन करके भाग्य की फसल मिलती है। इस प्रकार भाग्य आपकी अपनी रचना है। आपने ही इसे बनाया है। श्रेष्ठ विचारों को प्रश्रय दे कर, सत्कर्म करके तथा अपने सोचने के ढंग को बदल आप अपने भाग्य को निरस्त कर सकते हैं। अभी आप सोचते हैं कि आप शरीर है और आपका अमुक नाम है। अब इसके विपरीत सोचना प्रारम्भ करें। विचार करें कि आप सर्वव्यापक अमर ब्रह्म हैं। आप ब्रह्म ही हो जायेंगे। यह अपरिवर्त्य नियम है।
तीन प्रकार के कर्म
संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण
कर्म तीन प्रकार के होते हैं-संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण अथवा आगामी। अतीत के एकत्रित कर्म संचित कहलाते हैं। इनका एक अंश मनुष्य के चरित्र, उसकी प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों, झुकावों, क्षमताओं, इच्छाओं आदि में दृष्टिगोचर होता है। संचित कर्मों से ही प्रवृत्तियाँ उद्भूत होती हैं। प्रारब्ध भूत कर्मों का वह अंश है जो वर्तमान शरीर के लिए उत्तरदायी है। संचित कर्मों का वह अंश जिससे वर्तमान जन्म प्रभावित होता है, प्रारब्ध कहलाता है। यह पकी हुई फसल के समान है। इससे न बचा जा सकता है और न इसे बदला जा सकता है। इसे भोग करके ही क्षय किया जा सकता है। आप अपना पुराना ऋण चुकाते हैं। प्रारब्ध कर्म वह है, जो आरम्भ हो गया है और वस्तुतः फल प्रदान कर रहा है। संचित कर्मों के ढेर में से उसे चुना जाता है। क्रियमाण कर्म वह है जो भविष्य के लिए निर्मित हो रहा है-इसे आगामी अथवा वर्तमान भी कहते हैं।
वेदान्त-साहित्य में एक सुन्दर सादृश्य प्रस्तुत किया गया है। धनुर्धर ने तीर छोड़ दिया है, उसके हाथ से तीर छूट चुका है, वह उसे वापस नहीं लौटा सकता। अब वह दूसरा बाण छोड़ने वाला है। उसकी पीठ पर रखे हुए तरकश में बाणों का ढेर संचित कर्म है; जो बाण उसने छोड़ दिया, वह प्रारब्ध है और जो बाण वह छोड़ने वाला है, वह आगामी कर्म है। इसमें से संचित और आगामी पर उसका पूर्णाधिकार है; परन्तु प्रारब्ध उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अतीत के जो कर्म परिपक्व हो गये हैं, उन्हें उसको भोगना ही पड़ेगा।
एक अन्य सुन्दर सादृश्य भी है। अन्न भण्डार संचित कर्म है। अन्न-भण्डार का जो भाग बिक्री हेतु दुकान पर रख दिया जाता है, वह प्रारब्ध कर्म है और जो भाग नित्य बेचा जाता है, वह आगामी कर्म का प्रतिनिधित्व करता है।
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने से संचित कर्म-समूह नष्ट हो जाता है। श्रेष्ठ और दिव्य विचारों को प्रश्रय देने एवं सत्कर्मों को करने से उसमें बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। आगामी कर्म प्रायश्चित्त द्वारा, निमित्त-भाव (अर्थात् इस भाव से कि मनुष्य परमात्मा के हाथ का यन्त्र मात्र है) द्वारा तथा साक्षी-भाव (यह भाव कि व्यक्ति मन और इन्द्रियों के कर्मों का साक्षी मात्र है) से नष्ट किये जा सकते हैं।
स्वतन्त्र इच्छा की सर्वोच्चता
आप अपनी नियति के स्वामी हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप जो-कुछ दुःख प्राप्त करते हैं, उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। यदि आप सुखी हैं, तो अपने कर्मों के कारण और यदि दुःखी हैं तो भी अपने कर्मों के कारण। प्रत्येक कर्म का फल देर-सबेर अवश्य मिलता है। सत्कर्म का परिणाम सुखद होता है तथा दुष्कर्म का दुःखद।
आपको भोग-स्वातन्त्र्य का नहीं, वरन् कर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार है। इसलिए भगवान् कृष्ण ने कहा है : "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन-कर्म करने का ही तेरा अधिकार है, कर्म-फल पर नहीं।" जनकादि ने कर्म के द्वारा ही पूर्णता प्राप्त की थी। आप अपने चरित्र, विचार और कामनाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। मनुष्य की इच्छा सदा स्वतन्त्र है। स्वार्थपरायणता के कारण उसकी इच्छा दूषित हो गयी है। निम्न कामनाओं एवं रुचि-अरुचि से मुक्ति पा कर वह अपनी इच्छा को शुद्ध, दृढ़ और सक्रिय बना सकता है। प्रत्येक आत्मा एक ऐसे कृषक की भाँति है जिसके पास अपनी भूमि का एक टुकड़ा है। भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की प्रकृति, ऋतु की परिस्थितियाँ आदि सब पहले ही निश्चय हो चुकती हैं। परन्तु कृषक इस बात के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है कि वह भूमि को जोत कर और खाद दे कर अच्छी फसल प्राप्त करे या उसे अकृष्ट रहने दे।
जो-कुछ आप वर्तमान में हैं, वह भूतकाल के आपके विचारों और कर्मों का फल है। जो-कुछ आप भविष्य में बनेंगे, वह आपके वर्तमान विचारों और कर्मों का परिणाम होगा। जो प्रवृत्तियाँ आपने पूर्व जन्म में प्राप्त की थीं, उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त वातावरण आपको वर्तमान में प्राप्त होता है। भविष्य के लिए आप अपेक्षाकृत उत्तम परिस्थितियाँ बना सकते हैं। आप अपने इच्छानुसार कर्मों को रूप दे सकते हैं। आप पूर्णता की बहुत ऊँची स्थिति तक उठ सकते हैं। आप इन्द्र या पूर्ण योगी बन सकते हैं। आप अपना चरित्र, विचार और कर्म बदल सकते हैं। इसलिए भीष्म और वसिष्ठ ने पुरुषार्थ को भाग्य से उच्चतर स्थान दिया है।
जिस नाविक के पास डाँड, पतवार तथा पाल नहीं होते, उसे हवाएँ और तरंगें कहाँ-की-कहाँ बहा ले जाती हैं; किन्तु जिस निपुण नाविक के पास ये वस्तुएँ होती हैं, वह अपनी नौका को किसी भी इच्छित दिशा में ले जा सकता है तथा दूसरे किनारे पर कुशलतापूर्वक पहुँचा सकता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को प्रकृति का नियम-विचार का नियम, कर्म का नियम और कारण कार्य का नियम-ज्ञात है, बह इस संसार-समुद्र को निर्भीकतापूर्वक पार करके निर्भयता एवं अमरता के दूसरे तट पर पूर्ण कुशलतापूर्वक पहुँच सकता है। इन नियमों के ज्ञान की सहायता ले कर वह सहायक शक्तियों से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से उनका (शक्तियों का) उपयोग करेगा और विरोधी तत्त्वों को कुशलता से निष्प्रभावी कर देगा। ज्ञान प्रकाश-स्तम्भ है। अतः ज्ञान नितान्त आवश्यक है। अज्ञानता महान् पाप है। अज्ञानी मनुष्य प्रकृति का शिकार या दास बन जाता है।
निष्काम कर्म की महिमा
स्वार्थपूर्ण कर्म मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण है। पुनर्जन्म पुराने कर्मों को भोगते हुए नये कर्मों को जन्म देता है। पुनर्जन्म के दुःखों से मुक्त होने के लिए कर्म से मुक्त होना होगा। निष्काम कर्म आपको बन्धन में नहीं डालेगा। वह आपके हृदय को शुद्ध बनायेगा और ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करेगा जिसके कारण आपके ऊपर दिव्य प्रकाश तथा भगवत्प्रसाद का अवतरण होगा। सम्यक् चिन्तन करें, भद्रतापूर्वक कार्य करें, नियमित रूप से ध्यान करें और शाश्वत परमानन्द तथा अमरता प्राप्त करें!
पुनर्जन्म का सिद्धान्त
पुनर्जन्म अर्थात् आत्मा के आवागमन का सिद्धान्त हिन्दू-धर्म का आधारभूत सिद्धान्त है। पुनर्जन्म का शाब्दिक अर्थ है-पुनः मूर्त रूप में आना अर्थात् स्थूल शरीर को पुनः धारण करना। जीवात्मा पुनः एक मांसल आवरण ग्रहण करता है। आवागमन शब्द का अर्थ है- एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, नये संसार में प्रवेश करना।
संस्कृत शब्द 'संसार' संस्कृत धातु 'सृ' से निकला है जिसका अर्थ है-संसरण करना। उपसर्ग 'सम्' का अर्थ-अत्यधिक। जीवात्मा बारम्बार इस संसार में और अन्य सूक्ष्म उच्चतर लोकों में संसरण करता रहता है। आत्मा का इस प्रकार बार-बार संसरण ही संसार का वास्तविक अर्थ है।
संसार का अस्तित्व इसलिए है ताकि जीवात्मा आत्म-साक्षात्कार कर सके।।
मानव में असीम सम्भावनाएँ निहित हैं। शक्ति और बुद्धि का भण्डार उसके भीतर है। उसे अपनी अन्तर्निहित दिव्यता को प्रकट करना होगा। जीवन और मृत्यु से गुजरने का यही उद्देश्य है।
हिन्दू-धर्मग्रन्थों में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का निरूपण
मृत्यु के पश्चात् आपका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। वर्तमान जीवन के पूर्व आपने असंख्य जीवन व्यतीत किये हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है-"अर्जुना इससे पूर्व तुमने और मैंने कई जन्म लिये हैं। केवल में ही उनके विषय में जानता है। तुम नहीं जानते। जन्म के बाद मृत्यु होना अनिवार्य है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नये वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शरीर में वास करने वाला आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नये शरीरों में प्रवेश करता है।"
उपनिषदों ने भी घोषित किया है- "जिस प्रकार एक जोंक एक तृण के अन्त में पहुँच कर दूसरे तृण-रूप आश्रय को पकड़ कर अपने को सिकोड़ लेती है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को मार कर-अविद्या (अचेतनावस्था) को प्राप्त कर दूसरे आधार का आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है" (बृहदारण्यक उपनिषद् : ४/४/३)। "जिस प्रकार सुनार सोने का एक टुकड़ा ले कर उससे दूसरे नवीन और अधिक सुन्दर रूप की रचना करता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को नष्ट कर-अचेतनावस्था को प्राप्त करा कर अन्य पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा अन्य भूतों के नवीन और सुन्दर रूप की रचना करता है" (बृहदारण्यक उपनिषद् : ४/४/४)। "अन्न की भाँति मनुष्य पकता है (अर्थात् जराजीर्ण हो कर मर जाता है) तथा अन्न की भाँति ही वह (कर्मवश) पुनः जन्म ले लेता है" (कठोपनिषद् : १/१/६)।
कर्म और पुनर्जन्म
पुनर्जन्म का सिद्धान्त कर्म के सिद्धान्त का ही उपसिद्धान्त है। एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति की प्रकृति में जो भेद पाया जाता है, वह उनके अपने पूर्व-कर्मों के कारण ही होगा। पूर्व-कर्म का अर्थ है पूर्व-जन्म। इसके अतिरिक्त आपके समस्त कर्मों का फल इसी जीवन में नहीं मिल सकता, इसलिए अवशिष्ट कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए एक और जन्म होना चाहिए। प्रत्येक आत्मा बहुत बार जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त होता है। जब तक आप अविनाशी परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक जन्म और मृत्यु की श्रृंखला समाप्त नहीं होगी।
अच्छे कर्म उच्च योनियों में जन्म लेने के तथा बुरे कर्म नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनते हैं। सदाचरण करने से उच्च लोकों की ओर ऊर्ध्वगमन होता है तथा दुराचरण करने से निम्न लोकों की ओर अधोगमन। विद्या का परिणाम मोक्ष है और इसके विपरीत (अविद्या) का परिणाम बन्धन है। जब तक अच्छे तथा बुरे कर्म नष्ट नहीं होते, मनुष्य सैकड़ों कल्पों में भी मोक्ष या कैवल्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छे और बुरे-दोनों प्रकार के कर्म जीव को अपनी जंजीर में मजबूती से बाँध कर रखते हैं। एक जंजीर स्वर्ण की है और दूसरी लौह की। शाश्वत तत्त्व का ज्ञान प्राप्त किये बिना मनुष्य के द्वारा मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता।
पूर्व-जन्मों के अस्तित्व के प्रमाण
नवजात शिशु हर्ष, भय और दुःख प्रकट करता है। इसका कारण तब तक समझ में नहीं आ सकता, जब तक कि हम यह न मानें कि शिशु इस जीवन में कुछ चीजों को देख कर पूर्व-जीवन की तत्सदृश वस्तुओं की याद करता है। जो वस्तुएँ पहले हर्ष, भय और दुःख उत्पन्न किया करती थीं, वे इस जीवन में भी उसी प्रकार हर्ष, भय आदि उत्पन्न करती रहती हैं। भूतकाल की स्मृति पूर्व-जन्म को तथा आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है।
नवजात शिशु क्षुधा शान्त करने के लिए माँ का दूध पीता है। पूर्व-जन्म में इसी प्रकार करने की स्मृति बनी रहने के कारण वह ऐसा करता है। बच्चे को दूध पीने की इच्छा उसके पूर्व-जन्म के अनुभव के कारण होती है। इससे यह सिद्ध है कि यद्यपि शिशु की आत्मा ने पूर्व-शरीर त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लिया है; परन्तु उसे पूर्व-जन्म के शरीर के अनुभवों का स्मरण है।
आप संसार में नितान्त विस्मरणशीलता की अवस्था तथा निपट अन्धकार में भटकते हुए नहीं आये हैं। आप पूर्व-जन्म में प्राप्त की हुई कुछ आदतें और स्मृतियाँ ले कर जन्म लेते हैं। इच्छाएँ पूर्व-अनुभव से उद्भूत होती हैं। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना इच्छा के उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक प्राणी कुछ इच्छाओं को ले कर उत्पन्न होता है जिनका सम्बन्ध उसके पूर्व-जन्म में भोगी हुई वस्तुओं से होता है। इच्छाएँ पूर्व-जन्मों में उसके आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं।
मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य आत्मा का मार्ग
आत्मा सूक्ष्म शरीर (लिंग-देह) के साथ उत्क्रमण करती है। सूक्ष्म शरीर इन उन्नीस तत्त्वों से निर्मित है-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जीवात्मा के समस्त संस्कार, वासनाएँ और वृत्तियाँ इस सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती हैं। सूक्ष्म शरीर फिर स्वर्ग की ओर चल देता है। जब शुभ कमों के फल समाप्त हो जाते हैं, तब यह अपने लिए नया शरीर तैयार करके पृथ्वीच पुनः जन्म लेता है।
जिनका आचरण अच्छा रहा है, वे उच्च योनियों में जन्म लेते हैं और जिसका आचरण अच्छा नहीं रहता, वे पाप-योनियों अथवा निम्न कोटि की योनियों में कच लेते हैं।
देवयान और पितृयान
ध्यान और उपासना करने वाला व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो प्रथमत वह प्रकाश में जाता है, फिर वह प्रकाश से दिवस को, दिवस से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के छह मास को, उत्तरायण से वर्ष को, वर्ष से सूर्य को, सूर्य से चन्द्रमा को तथा चन्द्रमा से विद्युत् को जाता है। विद्युत् के क्षेत्र में पहुँच कर वह ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो मानव नहीं है। वह व्यक्ति उसे कार्यब्रह्म अर्थात् हिरण्यगर्भ के पास ले जाता है। यह देवों का मार्ग अर्थात् देवयान है।
लोकहित के काम करने वाला तथा दान करने वाला व्यक्ति मृत्यूपरान्त प्रथमतः धूम्रलोक को जाता है, फिर वह धूम्रलोक से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण पक्ष को, कृष्णण पक्ष से दक्षिणायन को और वहाँ से वह पितृलोक को जाता है। पितृलोक से बह आकाश को तथा आकाश से चन्द्रमा को जाता है। वहाँ वह पुण्य कर्मों के क्षीण होने तक रहता है। पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर वह फिर इसी मार्ग से इस पृथ्वी पर लौट आता है। पहले वह आकाश बनता है, फिर वायु, फिर धुआँ, फिर कोहरा, फिर मेध और तब वर्षा की बूँदों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। तब वह भोजन में प्रवेश करता है जिसे मनुष्य खाते हैं। अन्ततः वह उनकी सन्तान बन जाता है।
वह खनिज-जगत्, वनस्पति-जगत् और पशु-जगत् के विभिन्न अस्तित्वों को पार करता है अर्थात् जरायुज (जरायु से उत्पन्न) बनने से पूर्व वह उद्भिज (बीज से उत्पन्न), स्वेदज (स्वेद से उत्पन्न) और अण्डज (अण्डे से उत्पन्न) बनता है।
संसार के बन्धन को किस प्रकार तोड़ें
इस संसार-चक्र अथवा भव-चक्र अथवा जन्म-मृत्यु-चक्र में बाँधने वाली जंजीरें आपकी इच्छाएँ ही हैं। जब तक आप इस संसार के पदार्थों की इच्छा करते रहेंगे, तब तक आपको उन्हें प्राप्त करके भोगने के लिए इस संसार में आना ही पड़ेगा। किन्तु जब इन भौतिक पदार्थों के लिए आपकी कामना समाप्त हो जायेगी, तब बन्धन टूट जायेंगे और आप स्वतन्त्र हो जायेंगे। फिर आपको अन्य जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जायेगी।
आप इस संसार में भटकते हैं, क्योंकि आप अपने को परमात्मा से भिन्न समझते हैं। ध्यान और योग के द्वारा यदि आप अपने-आपको 'उसके साथ एक कर दें, तो आप अमरता और शाश्वत परमानन्द प्राप्त करेंगे। शाश्वत तत्त्व के ज्ञान द्वारा कर्म के बन्धन को काट कर अपनी अन्तरात्मा-जो अन्तर्यामी है-की परम शान्ति का अनुभव करें। आप जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जायेंगे। पापों और दुर्वासनाओं से मुक्त हो कर आप जीवन्मुक्त बन जायेंगे। आप सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करेंगे तथा 'उसे' सभी जीवों के रूप में देखेंगे।
अवतार की अवधारणा
मनुष्य के आरोहण के लिए परमात्मा का पृथ्वी पर अवरोहण अवतार कहलाता है। गीता में भगवान् कृष्ण कहते हैं- "यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशीस्वरूप तथा सब भूत-प्राणियों का ईश्वर हूँ, तदपि मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योगमाया से प्रकट होता हूँ। जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म-स्थापना के लिए युग-युग में प्रकट होता हूँ" (४/६, ७ और ८)।
ईश-कृपा का सिद्धान्त
भागवतों के अपने निजी शास्त्र हैं। इन्हें पांचरात्र आगम कहते हैं। इनमें वासुदेव-मत को प्रतिपादित किया गया है-इसलिए वे उपनिषदों के समकक्ष समझे जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित धर्म पथभ्रष्ट मानवता के लिए उपलब्ध ईश-कृपा पर आधारित है। इसलिए इस धर्म में अवतार के सिद्धान्त पर अधिक बल दिया गया है और उन अमर कथाओं का प्रचार किया गया है जो बाद में विष्णुपुराण, हरिवंशपुराण और भागवतपुराण में संकलित की गयीं। इन ग्रन्थों को पढ़ने से आपको भगवान् कृष्ण की महिमा का स्पष्ट ज्ञान होगा।
भगवान् कृष्ण, राम आदि अवतारों की उपासना द्वारा आपको आत्मसाक्षात्कार हो सकता है। बहुतों ने पहले से ही आत्मासाक्षात्कार प्राप्त कर लिया। तुकाराम, रामदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि ने परमात्मा का आमने-सामने दर्शन किया है। उनकी सशक्त रचनाओं से उनकी उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों का परिवा प्राप्त होता है।
ईश्वर-अभिव्यक्ति की श्रेणियाँ
पूर्णावतार, अंशावतार और आवेशावतार-ये अवतारों के प्रकार हैं। भगवान् कृष्ण की कलाओं की संख्या १६ है। वे पूर्णावतार हैं। उन्होंने मानवीय प्राणी के समान न जन्म लिया और न मृत्यु को प्राप्त हुए। वे प्रकट हुए और अन्तर्धान हो गये। वे अब भी हैं। उनकी नित्य-लीलाएँ गोलोक (अर्थात् दिव्य वृन्दावन) में हुआ करती हैं। अवतारों के शरीर दिव्य अर्थात् अप्राकृत होते हैं। उनके शरीर मानवीय हाड़-मांस से नहीं बने होते।
केवल अज्ञानी तथा भ्रमित आत्माएँ अवतार-सिद्धान्त का विरोध करती हैं और यह मानती है कि भगवान् कृष्ण मात्र मनुष्य थे। उन्होंने पवित्र धर्मग्रन्थों का भी प्रकार अध्ययन नहीं किया है। वे अल्प बुद्धि के तामसी लोग हैं। वे छिद्रान्वेषण करने में ही रुचि रखते हैं। भगवान् कृष्ण कहते हैं- "दुष्कर्मों में रत भ्रमित तथा दुष्ट मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं होते। माया उनकी बुद्धि को नष्ट कर देती है। वे दानवी स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसा उनका भाग्य होता है।"
बन्धुओ ! आप सम्पूर्ण हृदय तथा मन से राम या कृष्ण की उपासना करें। उन्हें अपने हृदय में प्रतिष्ठित करें। वह शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे और आप उनकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे। आप अमरता और शाश्वत परमानन्द प्राप्त करेंगे। अवतारों की जय हो! भगवान् विष्णु के अवतारों भगवान् राम और भगवान् कृष्ण की जय हो! उनका अनुग्रह आप सब पर रहे!
षष्ठ अध्याय
हिन्दू-कर्मकाण्ड
सन्ध्योपासना
सन्ध्योपासना का शाब्दिक अर्थ है-दो बेलाओं के सन्धि-काल में उपासना। यह रात्रि तथा दिवस, पूर्वाह्न तथा अपराह्न एवं सन्ध्या तथा रात्रि के सन्धि-कालों में की जाने वाली प्रभु की प्रार्थना तथा उपासना है। सूर्य को अर्घ्य देना एवं गायत्री-मन्त्र का जप तथा उपासना करना इसके मूलभूत अंग हैं। वस्तुतः उपर्युक्त बेलाओं में की गयी प्रत्येक सन्ध्योपासना उपासक की दिनचर्या की अवधि में किये पापों के लिए, क्षमा एवं ज्ञान तथा दैवी कृपा की सम्प्राप्ति के लिए भगवान् से की गयी प्रार्थना है।
समुचित सन्धि-काल में सन्ध्योपासना करने से ही अधिक लाभ होता है। सन्धि-काल में शक्ति का विशेष स्फुरण होता है। सन्ध्या-काल की समाप्ति के पश्चात् यह शक्ति लुप्त हो जाती है।
एक अनिवार्य कर्तव्य
जिस हिन्दू का यज्ञोपवीत-संस्कार सम्पन्न हो चुका है, उसके लिए सन्ध्योपासना एक दैनिक धार्मिक कृत्य है। यह एक नित्य कर्म है। सन्ध्योपासना एक अनिवार्य कर्तव्य है जिसे आत्म-शुद्धि तथा आत्मोन्नति के लिए प्रतिदिन करना चाहिए।
सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को सन्ध्योपासना करनी चाहिए। प्रत्येक ब्रह्मचारी तथा प्रत्येक गृहस्थ का यह दैनिक कर्तव्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो वह प्रत्यवाय-दोष का भागी होता है और उसका ब्रह्म-तेज नष्ट हो जाता है।
हिन्दू-शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी ब्राह्मण, जो भी क्षत्रिय या जो भी वैश्य प्रतिदिन त्रिकाल सन्ध्योपासना नहीं करता, वह नरकगामी होता है। याज्ञवल्क्यस्मृति में केवल सन्ध्योपासना के प्रयोजन के लिए ही यज्ञोपवीत-संस्कार का विधान निर्धारित किया गया है। इस विधान के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्वारा यज्ञोपवीत धारण करने की आयु क्रमशः आठ, ग्यारह तथा बारह वर्ष की है; क्योंकि इस संस्कार-विशेष के पश्चात् ही उन्हें सन्ध्या तथा वैदिक अनुष्ठानों का पात्र समझा जाता है। उन्हें बाह्याभ्यन्तर रूप से स्वयं को शुद्ध रखना चाहिए। तभी वे दैवी विज्ञान की पावन महिमा से सुपरिचित हो सकते हैं।
सन्ध्योपासना के लाभ
जप, उपासना, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम आदि का संयुक्त रूप सन्ध्या है। जो नित्य-प्रति सन्ध्या करता है, उसका मुखमण्डल ब्रह्म-तेज से उद्दीप्त रहता है, जो व्यक्ति निर्धारित विधि से शास्त्र-सम्मत समय पर नित्य-प्रति घ्यार करता है, वह विशुद्ध हो जाता है और उसका प्रत्येक प्रयत्न सफल होता है। उसे शक्ति तथा शान्ति की सम्प्राप्ति होती है। नियमित सन्ध्या पूर्व-संचित संस्कारों के पाश को विच्छिन्न कर प्रत्येक व्यक्ति की पुरातन परिस्थिति को पूर्णतः परिवर्तित कर देती है। इससे शुचिता, आत्मभाव, भक्ति एवं निष्कपटता का उदय होता है।
अनुष्ठान-विधि
आचमन, मार्जन, अघमर्षण, सूर्य-अर्घ्य, प्राणायाम, गायत्री मन्त्र का मौन जप एवं उपस्थान इस अनुष्ठान के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। आचमन में 'अच्युताय नमः', 'अनन्ताय नमः', 'गोविन्दाय नमः' इत्यादि मन्त्रों से अभिषिक्त जल का अधर से स्पर्श कराया जाता है और मार्जन में शरीर तथा मन की शुद्धि के लिए शरीर पर जल छिड़का जाता है। सूर्य-अर्घ्य में सूर्य देवता तो जल अर्पित किया जाता है और प्राणायाम के द्वारा श्वास-प्रश्वास को नियन्त्रित कर चंचल मन को स्थिर किया जाता है।
अर्घ्य
अर्घ्य तक के प्रथम चरण में जल को सम्बोधित स्तोत्र तथा उससे प्राप्त लाभों का उल्लेख है। मुख तथा शिर पर जल छिड़क कर भीगी उँगलियों से मुख, नासिका, कर्ण, वक्ष, स्कन्ध, शिर आदि विभिन्न अंगों के स्पर्श का प्रयोजन उक्त अंगों का पवित्रीकरण तथा इनके अधिष्ठातृदेवों का आवाहन है। इससे स्नायुकेन्द्र उद्दीप्त तथा सुप्त शक्तियाँ जाग्रत होती हैं।
अर्घ्य उन दैत्यों को दूर भगाता है जो उगते हुए सूर्य का मार्ग अवरुद्ध करते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि काम, क्रोध तथा लोभ वे दैत्य है जो बुद्धि के विकास में बाधा उपस्थित करते हैं। बुद्धि ही सूर्य है।
प्राणायाम तथा जप
सन्ध्या का द्वितीय चरण प्राणायाम तथा गायत्री जप है।
सूर्योपस्थान
सूर्योपस्थान सन्ध्या का तृतीय चरण है। यह क्षमा, दया तथा भगवत्कृपा के निमित्त की जाने वाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना में कहा गया है-"मुझे भूलोक में स्खलित मत होने दो। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। मेरी शक्ति अत्यन्त क्षीण थी। हे भगवन्! मैंने कुकृत्य किये हैं। हे प्रभु, मुझ पर दया करो।" यह प्रातः, मध्याह्न तथा सान्ध्य प्रहर में सूर्यदेव को सम्बोधित-निवेदित वेद की ऋचाएँ हैं। सूर्य मनुष्य की बुद्धि है तथा अज्ञान अन्धकार है। ज्ञान प्रकाश है। जब आप अज्ञान के अन्धकार से मुक्त हो जाते हैं और जब वेद माता गायत्री की कृपा से आपकी अन्तःप्रज्ञा के चक्षु खुल जाते हैं, तब आपको शाश्वत आनन्द, चरम शान्ति तथा अमरत्व की सम्प्राप्ति हो जाती है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो अज्ञान के अन्धकार तथा विक्षेप को नष्ट कर देता है; यह वह वन्दनीय दीप्ति है जिससे यह समस्त संसार ज्योतित है; यह वह पावन प्रकाश है जिसकी कृपा से भक्त का हृदय शाश्वत आनन्द से पूर्ण हो उठता है और यह वह सर्वोच्च ज्योति है जिसे साधक गायत्री मन्त्र के माध्यम से ईश्वर से प्राप्त करना चाहता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे ज्ञान प्रदान करे जिससे उसे आत्मसाक्षात्कार हो।
सन्ध्योपासना-एक सम्यक् विज्ञान
सत्य का साक्षात्कार मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। वह सृष्टि के रहस्य से परिचित होना चाहता है। इस सम्बन्ध में शास्त्रों की सुस्पष्ट उद्घोषणा है- "जब अज्ञान का नाश हो जाता है, जब पाखण्ड तथा मिथ्याचार विच्छिन्न हो जाते हैं और जब मनुष्य को उसकी हृदय-गुहा में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तभी उसके सम्मुख यथार्थ एवं अन्तिम सत्य अनावृत होता है।"
सत्य के राज्य में सफलता-प्राप्ति के लिए सन्ध्या-विज्ञान एक सम्यक् विज्ञान है। इस दैवी विज्ञान के अध्ययन में किसी को अपने मन में किसी प्रकार के अन्धविश्वास को स्थान नहीं देना चाहिए। किसी को इसकी महत्ता को सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसकी महत्ता एवं महिमा एक ज्वलन्त सत्य है। आज का भौतिकवादी समाज भी सन्ध्या-विज्ञान में निहित सत्य के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करता है। शास्त्रों में आया है- "ब्राह्मी-स्थिति वृक्ष, सन्ध्या इस वृक्ष का मूल, वेद इसकी शाखाएँ और धार्मिक कृत्य इसके पत्र हैं। अतः मूल अर्थात् सन्ध्या पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए।" अब सन्ध्या की महिमा सर्वथा स्पष्ट हो गयी। सत्य-मार्ग के पथिक के लिए सन्ध्या नितान्त आवश्यक है। शास्त्रों के समादेश के अनुसार ब्राह्मण को किसी भी मूल्य पर नियमित रूप से प्रतिदिन सन्ध्या करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी है-"अहरहः सन्ध्यामुपासीत।"
सन्ध्या के अभ्यास की पूर्वापेक्षाएँ
आहार
यदि आप इस विज्ञान में प्रशिक्षित होना चाहते हैं, तो आपको अपने भोजन के सम्बन्ध में अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। भोजन नियमित और सात्त्विक होना चाहिए। भोजन का मनुष्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आप एक छोटे शेर तथा बड़े हाथी के बीच के अन्तर को देखिए। समायोजित भोजन से आपका सम्यक् विकास होगा। विभिन्न प्रकार के गरिष्ठ भोजन से आलस्य उत्पन्न होता है। अतः आप अपने दैनिक भोजन-सम्बन्धी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन कीजिए। आपकी शक्ति एवं सक्रियता सर्वदा अक्षुण्ण रहेगी।
आसन (बैठने की मुद्रा)
जो व्यक्ति सन्ध्या करता है, वह आसन पर ध्यान नहीं देता। वह किसी भी मुद्रा में बैठ जाता है। यह अधिक लाभप्रद नहीं होता। उसे प्रतिदिन एक निश्चित दिशा की ओर उन्मुख हो कर किसी सम्यक् आसन (पद्मासन या सुखासन) में बैठना चाहिए। जहाँ तक हो सके, उसे एक ही बैठक में (अपने बैठने की मुद्रा को परिवर्तित किये बिना) अपनी सन्ध्योपासना समाप्त कर लेनी चाहिए। उसे आसन के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से दक्ष होना चाहिए, तभी वह सन्ध्योपासना करते समय अपने मन को एकाग्र कर सकेगा।
आस्था तथा भक्ति
आपको आस्था तथा भक्ति के साथ सन्ध्या करनी चाहिए। मन्त्र की आवृत्ति मात्र से विशेष लाभ नहीं होता। अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु से अन्तर्मन से प्रार्थना कीजिए।
युवा पीढ़ी से एक अनुरोध
कुसंस्कारों, भ्रान्तिपूर्ण शिक्षा-प्रणाली तथा कुसंग से ग्रस्त युवा छात्र सन्ध्या की महिमा तथा इसकी गहन प्रभावोत्पादकता को विस्मृत कर बैठे हैं। वे सन्ध्या नहीं करते। यह उनके लिए अर्थहीन हो चुकी है। वे नास्तिक हो गये हैं। वे सन्ध्या करने से पूर्व प्रयोगशाला में इसका परीक्षण तथा इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में विज्ञान-सम्मत प्रमाण चाहते हैं। उनके विचारानुसार पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा इसकी पुष्टि अनिवार्य है। प्राचीन ऋषियों के कथन का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। स्थिति कितनी पतनोन्मुखी है!
युवा छात्रो ! सन्ध्या की अवमानना कर स्वयं को विनष्ट मत कीजिए। सन्ध्या के दैनिक अनुष्ठान से आपका जीवन सफल होगा। इससे आपको भौतिक तथा आध्यात्मिक समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन एवं आन्तरिक शुद्धता की सम्प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त सन्ध्या आपके लिए ईश्वर-साक्षात्कार में भी सहायक सिद्ध होगी। अब से ही सही, इसका अनुष्ठान प्रारम्भ कर दीजिए। आप इसी क्षण उद्विमताओं एवं कठिनाइयों के बीच भी नियमित रूप से नित्यप्रति सन्ध्या करने का संकल्प कीजिए। विलम्ब मत कीजिए और अपने निरर्थक कार्यकलापों को कम कर दीजिए। वार्तालाप तथा मेल-जोल कम कीजिए। आपको सन्ध्या के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा।
सन्ध्या-सम्बन्धी अनुशासन का दृढ़तापूर्वक पालन कीजिए। वर्षा हो या झंझावात, यहाँ तक कि यदि प्रलय होने लगे, तो भी सन्ध्या को अधूरी मत छोड़िए। बहुत लोग कहते हैं कि सन्ध्या के लिए उन्हें समय नहीं मिल पाता है; क्योंकि उन्हें अन्य अनेक कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है, किन्तु इसका कारण उनकी दुर्बलता एवं उत्तम संस्कारों का अभाव ही है। वे इस दैवी विज्ञान की महिमा को नहीं समझ पाते। यदि वे अपने किसी मित्र को नदी के तट पर सन्ध्या की मुद्रा में बैठे देख लेते हैं, तो चिल्लाना या कोई आपत्तिजनक कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। उन अभागों को इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि सन्ध्या के मूल में कौन-सा गूढ़ तत्त्व निहित है। इस पवित्र अनुष्ठान में रहस्यों-का-रहस्य निहित है। इसी कारण प्राचीनकालीन ऋषि कहते थे - "जो व्यक्ति प्रतिदिन सन्ध्योपासना नहीं करता, वह वास्तव में पशु है।"
परमात्मा आपको किसी भी मूल्य पर प्रतिदिन सन्ध्या करने की बुद्धि प्रदान करे! आप सन्ध्या-सम्बन्धी नियमों का पालन करें। आप समस्त क्लेशों से मुक्त हों और पवित्र सन्ध्या-विज्ञान आपको विशुद्धता, अपरिमित आनन्द तथा अपरत्व प्रदान करे!
दश शास्त्रोक्त संस्कार
मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों के अनुरूप किये जाने वाले शास्त्र-विहित विशिष्ट कर्मों को संस्कार कहते हैं। मनुष्य के विशुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले ये शास्त्र-विहित कर्म हिन्दुओं के जीवन को पवित्र करते हैं। ये जन्म से ले कर मृत्युपर्यन्त व्यक्ति के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। ये मानव-जीवन की महत्त्वपूर्ण अवस्थाओं के विशेषक प्रतीक हैं। जिस प्रकार किसी चित्र की बहिरेखाओं को विभिन्न रंगों से अनुरंजित कर दिया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मण्य भी शास्त्रोक्त संस्कारों से तेजोमय हो उठता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था एवं मृत्यु से सम्बन्धित पृथक् पृथक् संस्कार होते हैं।
संस्कारों की कुल संख्या बावन है, जिनमें दश संस्कार महत्त्वपूर्ण हैं। ये दश मुख्य तथा मान्यता-प्राप्त संस्कार हैं- गर्भाधान, पुंसवन, सीमान्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन और विवाह। इन संस्कारों में भी अब कुछ ही प्रचलित रह गये हैं। कुछ संस्कार मनुष्य की अबोधावस्था एवं प्रारम्भिक शैशवावस्था से सम्बद्ध हैं। कुछ संस्कार ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हैं जिन्हें प्रतिदिन या विशिष्ट अवसरों पर सम्पन्न किया जाता है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक हिन्दुओं का पूरा जीवन महिमान्वित एवं सुरक्षित रहता है।
गर्भाधान
गर्भाधान प्रजनन-क्रिया को पवित्रता प्रदान करता है। इसमें पति शिशु के जन्म के लिए ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना करता है। वह ऋतु-शान्ति के अनुष्ठान या उत्सव के समय पवित्र मन्त्रों की आवृत्ति करता है और पत्नी इस मन्त्रपूत वातावरण में गर्भ धारण करती है। इससे भ्रूण के मस्तिष्क की कोशिकाओं में उत्तम संस्कार बन जाते हैं। शुद्ध बुद्धि एवं सम्यक् विवेक से सम्पन्न वास्तविक हिन्दू के लिए सम्भोग दैहिक सुख ही नहीं है। उस समय पुरुष अपनी दिव्य एवं रचनात्मक प्राणिक शक्ति का उपयोग एक मानव-शरीर के निर्माण के लिए कर रहा होता है। सम्भोग के समय पति-पत्नी को प्रफुल्ल-चित्त रहना चाहिए। अशान्ति, उद्विग्नता, क्रोध तथा घृणा की मनःस्थिति में उन्हें सम्भोग से विरत ही रहना चाहिए। उन्हें पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। यदि उनके मन में अर्जुन की प्रतिकृति उपस्थित होती है, तो उन्हें अभिमन्यु जैसे क्षात्रधर्मी एवं सुविज्ञ पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि उनके मन में भगवान् बुद्ध का चित्र प्रतिबिम्बित होता है, तो करुणा आदि सद्गुणों से सम्पन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि उनके मन में धन्वन्तरि की प्रतिकृति उपस्थित होती है, तो उन्हें प्राप्त पुत्र विख्यात आयुर्वेदाचार्य होता है। इसी प्रकार यदि उनकी मानसिकता का केन्द्र-बिन्दु सूर्यदेव होते हैं, तो उन्हें महिमा-मण्डित एवं दीप्तिमान् पुत्र की प्राप्ति होती है।
पुंसवन
तृतीय मास में पुंसवन-संस्कार होता है। इसके लिए कुछ मन्त्रों का विधान है। इस समय शिशु के अन्नमय-कोष तथा प्राणमय-कोष का निर्माण होता है।
सीमान्तोन्नयन
सीमान्तोन्नयन-संस्कार सप्तम मास में वेद-मन्त्रों के पाठ के साथ किया जाता है। यह अशुभ एवं अनिष्टकर शक्तियों के दुष्प्रभावों से माता की रक्षा करता है तथा गर्भस्थ शिशु को स्वास्थ्य प्रदान करता है। इससे शिशु के शरीर का सम्यक् विकास होता है। मन्त्रों के पाठ से निःसृत समस्वरतापूर्ण स्पन्दनों तथा इस संस्कार से सम्बन्धित अनुष्ठान के परिणामस्वरूप शिशु के शरीर का संगठन इस विधि से होता है कि वह सौन्दर्यमण्डित हो उठता है।
जातकर्म
शिशु के जन्मग्रहण के पश्चात् तत्क्षण ही जो संस्कार होता है, उसे जातकर्म कहते हैं। वह उसकी दीर्घायु, बुद्धि तथा कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और उसे शहद तथा मक्खन खिलाता है।
नामकरण
नामकरण-संस्कार (शिशु को नाम दिया जाना) मन्त्र-पाठ के साथ दशवें, ग्यारहवें या बारहवें दिन सम्पन्न होता है।
अन्नप्राशन
यह संस्कार छठे मास में सम्पन्न किया जाता है। इसमें शिशु को पहली बार ठोस भोज्य पदार्थ दिये जाते हैं। इस अवसर पर मन्त्र-पाठ होता है और विभिन्न देवों को नैवेद्य अर्पित किये जाते हैं।
चूड़ाकरण
चूड़ाकरण या मुण्डन-संस्कार प्रथम या तृतीय वर्ष में किया जाता है। कर्ण-वैध का अनुष्ठान प्रथम या सप्तम वर्ष में या प्रथम वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या चूड़ाकरण-संस्कार के साथ ही सम्पन्न होता है। इन अनुष्ठानों से शिशु का शरीर सन्तुलित रहता है और वीर्य तथा भ्रूण की विकृति के कारण उत्पन्न किसी भी पैतृक दोष का निराकरण हो जाता है। विद्यारम्भ भी एक संस्कार है जिसमें बालक को अक्षर-ज्ञान कराया जाता है। इसे अक्षराभ्यास भी कहते हैं। इन संस्कारों का सम्बन्ध जीवन की बाल्यावस्था से है।
उपनयन
जीवन की द्वितीय अवस्था अर्थात् युवावस्था से सम्बन्धित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान है-उपनयन-संस्कार। यह बालक का द्वितीय जन्म है जिसे आध्यात्मिक जीवन भी कहते हैं। उपनयन का अर्थ है-समीप ले जाना। इस अवसर पर बालक को गुरु के समीप उपस्थित किया जाता है। आचार्य उसे यज्ञोपवीत पहनाता है और गायत्री मन्त्र द्वारा दीक्षित कर उसे एक दण्ड प्रदान करता है। वह ब्रह्मचर्याश्रम का प्रारम्भ है जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। यहाँ से उसके अध्ययन-काल का प्रारम्भ होता है। इस दीक्षा के माध्यम से वह द्विज हो जाता है अर्थात् वह द्वितीय जन्म ग्रहण करता है। बालक का जन्म माता-पिता की पारस्परिक इच्छा से होता है। यह उसका भौतिक जन्म है। गायत्री मन्त्र में दीक्षित होने के पश्चात् उसका एक अन्य जन्म होता है और यही होता है उसका यथार्थ जन्म। याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का उपनयन संस्कार क्रमशः आठ, ग्यारह तथा बारह वर्ष की आयु में होता है। मनु के अनुसार यह आयु ब्राह्मण के लिए पाँच वर्ष, क्षत्रिय के लिए छह वर्ष तथा वैश्य के लिए आठ वर्ष है।
यज्ञोपवीत एवं अन्य प्रतीकों का महत्त्व
यज्ञोपवीत में एक-दूसरे से गुँथे हुए तीन धागे होते हैं। यज्ञोपवीतधारी को विचार, वाणी तथा शरीर अर्थात् मन-वचन-कर्म पर त्रिविध नियन्त्रण रखना चाहिए। यज्ञोपवीत विश्व में स्थित विभिन्न त्रिपुटियों जैसे सत्-चित्-आनन्द, सृष्टि-स्थिति-प्रलय, जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति (तीन अवस्थाएँ), सत्त्व-रजस्-तमस् (त्रिगुण) तथा ब्रह्मा-विष्णु-महेश (त्रिमूर्ति) आदि का संकेतक है।
दण्ड का यह निहितार्थ है कि विद्यार्थी को अपने मन, वचन और कर्म को नियन्त्रण में रखना चाहिए। जिसका इन तीनों पर नियन्त्रण है तथा जो मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, वह पूर्णता को प्राप्त होता है।
बालक एक कौपीन, एक छोटा पीत वस्त्र और कटि में मूँज निर्मित एक मेखला धारण करता है। आचार्य उस पर मृगचर्म रख देता है। उसका नवीन पीत वन नवीन देह का एवं पीत वर्ण आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कौपीन-धारण इस तथ्य की और संकेत करता है कि बालक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का विशुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेखला की लपेट त्रिविध होती है। इसका तात्पर्य यह है कि बालक के लिए संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषदों का अध्ययन आवश्यक है। मृगचर्म तपस्वी जीवन का संकेतक है-ऐसा ही जीवन उसे व्यतीत करना चाहिए।
समावर्तन
विद्यार्थी-जीवन की समाप्ति के पश्चात् जो संस्कार सम्पादित किया जाता है। उसे समावर्तन कहते हैं। विद्यार्थी वेदाध्ययन तथा व्रतों की समाप्ति के पश्चात् आचार्य को कुछ भेंट देता और औपचारिक स्नान की अनुमति प्राप्त करता है। यह स्नान उसके विद्यार्थी-जीवन के परिसमापन का प्रतीक है। घर लौटने पर उसका समावर्तन-संस्कार होता है। इस प्रकार अब वह विवाह कर जीवन की द्वितीय अवस्था अर्थात् गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए स्वयं को तत्पर पाता है।
विवाह
विवाह द्वारा मनुष्य का प्रवेश जीवन के द्वितीय आश्रम में होता है। यहीं से गृहस्थ-जीवन का प्रारम्भ होता है। वह मनुष्य के विहित कर्तव्यों का पालन करते हुए यज्ञ, स्वाध्याय तथा सन्तानोत्पत्ति द्वारा स्वयं को विभिन्न ऋणों से मुक्त करता है। वह (पति) वधू से कहता है- "मैं सौभाग्य के लिए पाणिग्रहण करता हूँ।" वे अपने हाथ में एक-दूसरे का हाथ ले कर पवित्र अग्नि की परिक्रमा करते हैं। नव-वधू अग्नि को धान्य की हवि प्रदान करते हुए यह प्रार्थना करती है- "मेरा पति दीर्घजीवी हो; मेरे कुटुम्ब की अभिवृद्धि हो।"
जीवन की अन्तिम दो अवस्थाएँ (आश्रम)
वानप्रस्थ एवं संन्यास, दो अन्य अवस्थाएँ हैं जिनके पृथक् पृथक् अनुष्ठान हैं। मनुष्य समस्त सांसारिक कर्मों का परित्याग कर वन में चला जाता है जहाँ वह स्वयं को संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। यह वानप्रस्थ का जीवन है।
संन्यासी संसार का परित्याग कर देता है और भिक्षा-वृत्ति ग्रहण कर स्वाध्याय तथा ध्यान का जीवन व्यतीत करता है।
प्रेतकर्म अन्त्येष्टि अर्थात् दाह-संस्कार को कहते हैं। यह उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जाता है।
पंच-महायज्ञ
शास्त्रों में पंच-महायज्ञों का विधान है जिन्हें गृहस्थ को प्रतिदिन सम्पन्न करना चाहिए। प्रथम ब्रह्म-यज्ञ है जिसे वेद-यज्ञ भी कहते हैं। इसमें ब्रह्म, वेदों या ऋषियों को हवि या समिधा अर्पित की जाती है। देव-यज्ञ द्वितीय यज्ञ है। इसमें देवों को हवि या समिधा अर्पित की जाती है। पितृ-यज्ञ तृतीय यज्ञ है जिसमें पितरों को हवि या समिधा अर्पित की जाती है। चतुर्थ यज्ञ भूत-यज्ञ है जिसमें समस्त प्राणियों को बलि अर्पित की जाती है। पंचम यज्ञ अर्थात् मनुष्य-यज्ञ में उपर्युक्त पदार्थ मनुष्य को प्रदान किये जाते हैं।
इन पंच-महायज्ञों का सम्पादन मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। वह क्रमिक रूप से इस तथ्य से परिचित हो जाता है कि वह एक पृथक् इकाई न हो कर इस विस्तृत ब्रह्माण्ड का एक अंग है। महान् ऋषियों द्वारा प्रणीत पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से उसे ज्ञान प्राप्त होता है। मित्रों, सम्बन्धियों और साथियों से उसे सहायता प्राप्त होती है। उसका भौतिक शरीर उसके माता-पिता द्वारा प्रदत्त होता है। इस शरीर का पोषण गो-दुग्ध, शाकादि वनस्पतियों एवं फलों से होता है। पंच-महाभूत उसकी सहायता करते हैं। वह आक्सीजन एवं जल के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। देव तथा पितर उसकी मंगल-कामना करते हैं। इस प्रकार प्रकृति का उस पर पंचविध ऋण होता है। अतः उसके लिए उक्त पंच-महायज्ञों के दैनिक सम्पादन द्वारा स्वयं को ऋण-मुक्त कर लेना अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त चलते समय, सफाई-बुहारन करते समय, खेत में धान्य काटते समय, खाद्यान्न पीसते समय और पाक-कर्मादि करते समय मनुष्य से अचेतन रूप में अनेक कृमि-कीटों की हत्या होती रहती है। इन पापों के निराकरण का माध्यम ये यज्ञ ही हैं।
पंच-यज्ञ
ऋषियों, देवों, पितरों, भूतों एवं अतिथियों को गृहस्थों से सहायता की अपेक्षा रहती है। अतः गृहस्थों को पंच-यज्ञों को नित्यप्रति सम्पन्न करना चाहिए। धर्मग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन करना ब्रह्म-यज्ञ है। पितरों को तर्पण तथा जलार्पण एवं श्राद्ध करना पितृ-यज्ञ है। होम करना या अनि को आहुति प्रदान करना देव-यज्ञ है। बलि देना या सर्वभूतों को खाद्यान्नार्पण करना भूत-यज्ञ है। अतिथि-सत्कार करना मनुष्य-यज्ञ या अतिथि-यज्ञ है।
ब्रह्म-यज्ञ या ऋषि-यज्ञ
प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन शास्त्राध्ययन करना चाहिए। उसे अन्य लोगों के साथ ज्ञान का आदान-प्रदान करना चाहिए। इसे ब्रह्म-यज्ञ या ऋषि-यज्ञ कहते हैं। इसके अनुष्ठान से वह ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाता है।
देव-यज्ञ
श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं- "कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ-सहित प्रजाओं को रच कर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त होओ। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे और इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवगण लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में (कर्तव्य समझ कर) उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होओगे। यज्ञ द्वारा बढ़ाये हुए देवता लोग तुम्हारे लिए (बिना माँगे ही) प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिये हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिये स्वयं ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। इसका कारण यह है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं और जो पापी लोग अपने शरीर-पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं" (अध्याय ३/१०, ११, १२ और १३)। मनु कहते हैं-"मनुष्य को वेदाध्ययन तथा देव-अनुष्ठानों में सर्वदा संलग्न रहना चाहिए। वेदोक्त अनुष्ठानों से वह चल एवं अचल जगत् का आधार स्तम्भ बन जाता है।" ये यज्ञ जीवन-चक्र को दैवी इच्छा के अनुरूप प्रवर्तित करते हैं। इस प्रकार मनुष्य तथा संसार के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।
पितृ-यज्ञ
पूर्वजों को नियमित रूप से तर्पण आदि अर्पित करना पितृ-यज्ञ है।
भूत-यज्ञ
गौ, श्वान, पक्षी, मत्स्यादि में भोजन-वितरण करने को भूत-यज्ञ कहते हैं।
मनुष्य-यज्ञ
निर्धनों को अन्न-दान करना मनुष्य-यज्ञ है। भूखों को भोजन, नंगों को वख, गृहविहीनों को शरण और दुःखी जनों को सुख देना इत्यादि कर्म मनुष्य-यज्ञ हैं। पीड़ित मानवता की किसी भी प्रकार की सेवा मनुष्य-यज्ञ है।
पंच-महायज्ञ के लाभ
प्रतिदिन दया तथा सहानुभूति से पूर्ण इन कार्यों को करने से मनुष्य के अन्तर में करुणा का विकास होता है। इससे घृणा नष्ट हो जाती है और मनुष्य का अहंकारपूर्ण हृदय क्रमशः कोमल होता जाता है। वह सार्विक प्रेम का धनी हो जाता है। उसका हृदय विस्तृत तथा जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। स्वार्थ और अहम्मन्यता से उत्पन्न उसकी पृथकता की पुरानी भावना क्रमशः क्षीणतर होती हुई अन्ततः सर्वथा विनष्ट हो जाती है। उसे इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि दूसरों को सुख दे करके, दूसरों की सेवा-सहायता करके, दूसरों के दुःखों को दूर करके और अपनी उपलब्धियों में दूसरों के भागीदार बना करके ही वह सुखी हो सकता है। नित्यप्रति किये जाने वाले पंच-महायज्ञों से उसे वरिष्ठ, समकक्ष तथा कनिष्ठ जनों से सम्यक् सम्बन्ध-स्थापन की शिक्षा मिलती है।
मनुष्य का कोई पृथक्, वैयक्तिक अस्तित्व नहीं होता। वह विश्व से सम्बद्ध है। वह माला में गूँथे एक दाने की भाँति है। उसका सारा जीवन यज्ञमय एवं कर्तव्यशील होना चाहिए। इसी विधि से मनुष्य का त्वरित विकास हो सकेगा, इसी विधि से उसे शाश्वत सत्ता के परमानन्द की अनुभूति हो सकेगी और इसी विधि से वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो कर अमरत्व प्राप्त कर सकेगा।
श्राद्ध और तर्पण
श्राद्ध जीव के भौतिक शरीर के परित्याग के पश्चात् उसकी शान्ति के लिए उसके सम्बन्धियों द्वारा किया जाने वाला संस्कार है। भौतिक कोष अर्थात् देह से मुक्त जीव को प्रेत कहते हैं। इस अवसर पर श्राद्ध के जिस अंश का सम्पादन किया जाता है, उसे प्रेत-क्रिया कहते हैं।
दिवंगत आत्मा को श्राद्ध तथा तर्पण से किस प्रकार लाभ पहुँचता है
पितरों के लाभार्थ सम्यक् समय तथा स्थान पर सुपात्र ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दान देने को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से पितरों को तुष्टि-लाभ होता है। पुत्र द्वारा श्राद्ध की सोलह आवृत्तियों के पश्चात् मृत पिता की आत्मा पितरों के सान्निध्य में सुखपूर्वक निवास करती है। अतः पुत्र को मृत पिता के लिए सपिण्डीकरण-अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध तथा तर्पण से पितृलोक की मृतात्मा की क्षुधा तथा पिपासा शान्त हो जाती है।
नरकगामी मृतात्माएँ क्षुधा-पिपासा से अत्यन्त पीड़ित रहती हैं। श्राद्ध-कर्म तथा चावल का पिण्ड-दान और तर्पण करके उन्हें कष्टमुक्त किया जाता है। अतः श्राद्ध-कर्म अनिवार्य है। जो मृतात्माएँ स्वर्ग में निवास करती हैं, उनको भी इससे तुष्टि, शक्ति तथा पोषण प्राप्त होता है।
श्राद्ध पितरों के सम्मान में किया जाने वाला एक अपरिहार्य अनुष्ठान है। इसे श्रद्धा, भक्ति तथा आदर के साथ सम्पन्न करना अत्यावश्यक है। जो पुत्र श्राद्ध तथा तर्पण नहीं करता, वह कृतघ्न पुत्र है। वह नरकगामी होता है। धर्मग्रन्थ उद्घोषित करते हैं-"जो श्राद्ध नहीं करता, उसका पुनर्जन्म निम्नतर योनियों में होता है। वह दुःखी तथा निर्धन जीवन व्यतीत करता है।"
दाह-संस्कार के लाभ
दाह-संस्कार मृतक की अन्त्येष्टि का सर्वोत्तम माध्यम है। यह मृतात्मा के लिए अत्यन्त लाभप्रद होता है। यदि मृतक का दाह-संस्कार नहीं होता, जो जीव पृथ्वी से ही सम्बद्ध रह जाता है। अपने भौतिक शरीर के प्रति मोह तथा आसक्ति के कारण वह उसके चतुर्दिक् मँडराता अथवा चक्कर लगाता रहता है और इस प्रकार स्वर्गलोक की उसकी दिव्य यात्रा में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। मन्त्र के स्वरों के स्पन्दन, आहुतियाँ तथा तर्पण दिवंगत आत्मा को सुख तथा सान्त्वना प्रदान करते हैं।
सपिण्डीकरण-अनुष्ठान जीव के प्रेत-लोक से पितृ-लोक की ओर प्रस्थान करने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार वह पितृ-लोक में पहुँच कर पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पुत्र पिता के शव की तीन बार प्रदक्षिणा करता है और 'तुम यहाँ से प्रस्थान करो' -इस मन्त्रोच्चारण के साथ उस पर एक बार जल छिड़कता है। दूसरे दिन अस्थियों को एकत्रित कर उन्हें किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। जो लोग समर्थ हैं, वे वाराणसी या हरिद्वार जा कर गंगा में अस्थि-विसर्जन करते हैं।
ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिस मृतक के देहावशेष को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, उसे आध्यात्मिक प्रकाश से आप्लावित उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है और अन्ततः वह मुक्त हो जाता है।
पितरों के दो वर्ग
मृत्यु के पश्चात् तत्क्षण जीव अग्नि, वायु तथा आकाश से निर्मित अतिवाहिक नामक देह धारण कर लेता है। इसके पश्चात् भू-लोक में उसके द्वारा सम्पन्न घोर पापों तथा पुण्यकर्मों के अनुरूप उसे नारकीय दुःखोपभोग के लिए यातना-देह तथा स्वर्गिक सुखोपभोग के लिए दिव्य देह की प्राप्ति होती है। यातना-देह वायु-तत्त्व-प्रधान एवं दिव्य देह अग्नि-तत्त्व-प्रधान होती है। जीव को पितृ-लोक में पहुँचने में एक वर्ष लगता है।
पितरों के दो वर्ग होते हैं। प्रथम वर्ग के पितरों को दिव्य पितर कहते हैं। ये पितृ-लोक के अधिपति होते हैं। द्वितीय वर्ग के पितरों को मानव-पितर कहा जाता है जो पितृ-लोक में मरणोपरान्त पहुँचते हैं। ब्रह्मा सभी का पितामह है। आदि प्रजननकर्ता होने के कारण कश्यप तथा अन्य प्रजापति भी पितर हैं। पितृ-लोक भुवर्लोक के नाम से जाना जाता है।
पितर शब्द का अर्थ मुख्यतः निकटतम पूर्वज-जैसे माता-पिता आदि-होता है। सम्यक् श्राद्ध पितरों की तीन पीढ़ियों या समस्त पितरों के लिए किया जाता है। पिता, पितामह तथा प्रपितामह को तीन पिण्ड अर्पित किये जाते हैं और सर्वप्रथम दो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। भोजन के आदान-प्रदान से सात पीढ़ियाँ पारस्परिक रूप से एक-दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं।
पितृ-पक्ष और महालया अमावस्या
आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष की संज्ञा दी गयी है। इस मास का यह पक्ष दिवंगत पूर्वजों को पिण्ड दान देने के लिए पवित्र एवं शास्त्र-सम्मत माना जाता है और जहाँ तक इस पक्ष के अन्तिम दिन का सम्बन्ध है, इसे अन्त्येष्टि जैसे संस्कारों के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है।
सामान्यतः आज भी परम्परावादी हिन्दू प्रत्येक अमावस्या को दिवंगतात्माओं के लिए अर्घ्य एवं तर्पण का अनुष्ठान किया करते हैं। शास्त्रानुमोदित अनुष्ठान भी मृत्यु-दिवस पर प्रत्येक वर्ष किये जाते हैं। इसे श्राद्ध कर्म कहा जाता है। इस स्थिति में इन अनुष्ठानों को विशेष रूप से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ही सम्पन्न करने का क्या महत्त्व है? वस्तुतः उक्त पक्ष में सम्पन्न किये जाने वाले अनुष्ठानों का प्रभाव अत्यधिक विशिष्ट होता है। भगवान् यम के एक वरदान के कारण ये आहुतियाँ पितरों तक तत्काल एवं प्रत्यक्ष रूप से पहुँच जाती हैं। वरदान का यह प्रसंग निम्नांकित है :
पितृ-पक्ष का उद्गम
महाभारत से उधृत एक कथा
महाभारत का प्रख्यात नायक दानवीर कर्ण अपने भौतिक शरीर के परित्याग के पश्चात् उच्चतर लोकों में ऊर्ध्वगमन करता हुआ योद्धाओं के लोक में पहुँचा। वहाँ जीवितावस्था में किये गये उसके असाधारण दान के पुण्य के फलस्वरूप उसे उसके दान से सहस्रगुना अधिक स्वर्ण तथा रजत के बृहद् भण्डार मिले। कर्ण की दान-राशि असीम थी, किन्तु उससे अन्न-दान की उपेक्षा हो गयी थी। इसके परिणामस्वरूप उसके चतुर्दिक् स्वर्ण तथा रजत की राशि तो एकत्र हो गयी; किन्तु उसकी तुष्टि के लिए उसे अन्न नहीं प्राप्त हो सका। उसने इसके लिए यमराज से प्रार्थना की। इसके प्रत्युत्तर में यमराज ने अन्न-दान की पूर्व-उपेक्षा के परिमार्जन के लिए उसे एक बार पुनः चौदह दिनों के लिए भू-लोक में भेज दिया। कर्ण मृत्यु-लोक में जा कर ब्राह्मणों तथा निर्धनों को चौदह दिनों तक भोजन कराता रहा। इसके अतिरिक्त उसने अन्तिम दिन महालया को जल-तर्पण एवं अन्य विहित अनुष्ठान भी किये। इस पक्ष के अन्तर्गत उसने भू-लोक में जो अनुष्ठान किये थे, उनके फलस्वरूप उसके अभावों का निराकरण हो गया। यह आश्विन मास का कृष्ण पक्ष था।
यमराज की कृपा से तब से एक ऐसी व्यवस्था का प्रचलन हो गया, जिसके अनुसार इस पक्ष-विशेष में किये गये इन अनुष्ठानों से निम्नांकित विलक्षण फल प्राप्त होने लगे। इस अवधि में दिया गया पिण्ड-दान सभी दिवंगत आत्माओं को, चाहे वे पारिवारिक दृष्टिकोण से पिण्ड-दान करने वाले व्यक्ति के प्रत्यक्ष सम्बन्धी हों या न हों, प्राप्त होने लगा। पितृ-पक्ष की अमावस्या को किया हुआ पिण्ड-दान निस्सन्तान व्यक्तियों की दिवंगत आत्माओं तक को प्राप्त होने लगा। जो लोग परोपकार तथा अन्न-दान के विरत रहते थे और इसके फलस्वरूप जिन्हें मरणोपरान्त पितृलोक में इन सुख-सुविधाओं से वंचित होना पड़ता था, वे भी इन अनुष्ठानों से लाभान्वित होने लगे। जिन लोगों की मरण-तिथि अज्ञात रहती है और जिन लोगों का वार्षिक श्राद्ध सम्पन्न नहीं हो पाता, उन्हें भी पितृ-पक्ष का पिण्ड-दान प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु भयंकर दुर्घटनाओं के कारण या अस्वाभाविक रूप से होती है और जिसके फलस्वरूप जिनकी दिवंगत आत्माएँ सामान्य रूप से पिण्ड-दान नहीं ग्रहण कर पातीं, उनको भी पितृ-पक्ष का पिण्ड-दान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। जबसे महान् कर्ण ने आश्विन पक्ष का यह अनुष्ठान प्रारम्भ किया, तभी से यमराज के उक्त वरदान फलित होने लगे। हिन्दू आज भी इस पक्ष के अनुष्ठान को अत्यधिक श्रद्धा और कठोर नियम के साथ सम्पन्न करते हैं। इस अवधि में वे प्रतिदिन तीन बार स्नान तथा आंशिक उपवास करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को सारे अनुष्ठानों का सम्पादन होता है और प्रचुर मात्रा में दान दिया जाता है।
दिवंगत आत्माओं की तुष्टि
महालया अमावस्या का दिन सभी हिन्दुओं के लिए महान् अर्थवत्ता और महत्त्व का दिन है। इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर पूर्वजों की दिवंगत आत्माओं की तुष्टि तथा शान्ति के लिए हार्दिक प्रार्थना की जाती है। हिन्दू-इतिहास के अनुसार महालया अमावस्या के दिन सूर्य तथा चन्द्रमा का परस्पर मिलन होता है और सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। उस दिन पितर हमारे पूर्वज यम-लोक-स्थित अपने निवास-स्थान का परित्याग कर मृत्यु-लोक में उतर आते हैं और अपने वंशधरों के घरों में निवास करते हैं।
अमावस्या से पूर्व का पक्ष अर्थात् प्रतिपदा से अमावस्या तक का काल पितरों की तुष्टि के लिए किये जाने वाले पवित्र अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। इस कृष्ण पक्ष में पितरों अर्थात् दिवंगत आत्माओं के सम्मान में किये जाने वाले अनुष्ठान गया में किये जाने वाले अनुष्ठानों के समकक्ष ही होते हैं। इन समस्त अनुष्ठानों का प्रयोजन पितरों का पूजन एवं उनकी इच्छाओं की तृप्ति है, ताकि वे वर्ष की शेष अवधि में शान्तिपूर्वक रह सकें।
नवरात्र या नौ-दिवसीय देवी-पूजन
धार्मिक अनुष्ठान, पारम्परिक पूजन एवं व्रत समयानुसार एक से अधिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हैं। ईश्वर की आराधना होने के अतिरिक्त ये जीवन्त अतीत के स्मरणोत्सव तथा रहस्यवादी निर्वचन के अनुसार लक्षणात्मक होते हैं। इसके अतिरिक्त से आत्म-साक्षात्कार के मार्ग पर जीव के विशिष्ट पथ-प्रदर्शक प्रकाश स्तम्भ भी हैं।
बाह्यतः देवी या माँ का नौ दिवसीय पूजन, जिसे नवरात्र-पूजा कहा जाता है, विजयोत्सव के रूप में प्रचलित है। शुम्भ-निशुम्भ के नेतृत्व में दुर्जेय राक्षसों द्वारा घोषित युद्ध में महाकाली की विजय के उपलक्ष्य में यह नौ-दिवसीय पूजा-अर्चा उन्हीं महाकाली को समर्पित की जाती है। किन्तु अपनी साधना की अवधि में महामाया के विभिन्न रूपों के पूजन के लिए आध्यात्मिक साधक द्वारा किये गये नौ रात्रियों के तीन भागों में विभाजन के मूल में जो सत्य निहित है, वह भव्य होने के साथ-साथ पूर्णतया व्यावहारिक भी है। ब्रह्माण्डीय स्तर पर इसका महत्त्व यह है कि यह मनुष्य के ईश्वर से सायुज्य या जीवत्व से शिवत्व की ओर विकास के विभिन्न चरणों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जहाँ तक इसके वैयक्तिक अभिप्राय या महत्त्व का सम्बन्ध है, यह व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना की अपेक्षित दिशा की ओर संकेत करता है।
मानवीय अस्तित्व का केन्द्रीय प्रयोजन सर्वोच्च सत्ता अर्थात् ब्रह्म से अपने शाश्वत तादात्म्य से परिचित होना तथा स्वयं को उस दिव्य सत्ता के अनुरूप विकसित करना है। सर्वोच्च सत्ता में आत्यन्तिक पूर्णता निहित है जो पूर्णतः विशुद्ध अर्थात् निरंजन है। उस सर्वोच्च सत्ता के साथ अपने सायुज्य से परिचित और उसके तद्रूप होना उस (सर्वोच्च) सत्ता के साथ निश्चित रूप से समस्वरता प्राप्त कर लेना है। अतः प्रारम्भ में साधक को उन असंख्य अशुद्धताओं तथा आसुरी तत्त्वों से मुक्त होना है जो उसके पार्थिव शरीर-धारण की अवस्था में उसके साथ चिपट गये हैं। इसके पश्चात् उसे उदात्त, शुभ एवं दिव्य गुण प्राप्त करने हैं। इस प्रकार उसके विशुद्ध हो जाने तथा सत्त्वगुण से सम्पन्न होने के पश्चात् वह ज्ञान की दीप्ति से उसी प्रकार उद्दीप्त हो उठता है जिस प्रकार किसी पूर्णतः शान्त सरोवर का पारदर्शी जल सूर्य की प्रोज्ज्वल किरणों से द्युतिमान् हो जाता है।
दुर्गा-पूजा पापों का निराकरण
साधना की इस प्रक्रिया में दृढ़ संकल्प, पूर्व-संकल्पित प्रयास तथा श्रमसाध्य संघर्ष की अपेक्षा है। दूसरे शब्दों में इसके लिए असीम शक्ति अपरिहार्य है। यह भगवती माँ (जो ब्रह्म की परा-शक्ति है) ही है जो साधक के माध्यम से क्रियाशील रहती है। प्रथम तीन दिनों तक माँ का पूजन विकराल शक्ति-रूपा दुर्गा के रूप में किया जाता है। आपमें जो कुछ भी अशुद्धता, पाप या दोष है, उसके निराकरण के लिए आप माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। यह साधक में विद्यमान पाशविक प्रवृत्ति एवं निम्नतर आसुरी प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष कर उसे नष्ट कर देती है। वह ऐसी महाशक्ति है जो आपकी साधना की उसमें उपस्थित होने वाली समस्त विघ्न-बाधाओं से रक्षा करती है। इस प्रकार प्रथम तीन दिनों का उपयोग बल अर्थात् काषाय की निवृत्ति तथा अनिष्टकर मानसिक वासनाओं के निराकरण के लिए किये जाने वाले संकल्पित प्रयास तथा संघर्ष के लिए होता है। यह नवरात्र का प्रथम चरण है जिसमें माँ के ध्वंसात्मक स्वरूप का पूजन होता है।
लक्ष्मी-पूजन सद्गुणों की सम्प्राप्ति
अशुद्ध वासनाओं, दुष्प्रवृत्तियों अर्थात् मनुष्य के निषेधात्मक पक्ष पर विजय-प्राप्ति के पश्चात् इनके स्थान पर रचनात्मक गुणों की सम्प्राप्ति के लिए है। इसके अन्तर्गत भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण द्वारा प्रोक्त दैवी सम्पदा अर्थात् दिव्य गुणों को प्राप्त करना पड़ता है। साधक के लिए यह अत्यावश्यक होता है कि वह इन समस्त सद्गुणों की प्राप्ति एवं इनके विकास के लिए प्रयास करता रहे। इस प्रयास में सफलता प्राप्त होने पर उसे दुर्लभ ज्ञानरत्न प्राप्त होता है। इस रत्न का मूल्य चुकाने के लिए उसे अपार आध्यात्मिक सम्पदा को एकत्र करना पड़ता है। विरोधी गुणों के विकास (प्रतिपक्ष भावना) के अभाव में आसुरी प्रकृति पुनः बलवती हो उठती है। अतः साधक की साधना के लिए यह द्वितीय चरण पूर्ववर्ती चरण की भाँति ही महत्त्वपूर्ण है। इन दोनों चरणों के बीच का मूलभूत अन्तर यह है कि जहाँ प्रथम चरण में अपने व्यक्तित्व के मलिन एवं अहम्मन्यतापूर्ण निम्नतर पक्ष का संकल्पित भाव से निष्ठुरतापूर्वक दमन करना पड़ता है वहाँ द्वितीय चरण में शुचिता के विकास के लिए सुसम्बद्ध तथा सन्तुलित प्रयास करने पड़ते हैं। साधक की साधना के इस रमणीयतर पक्ष का चित्रांकन माँ लक्ष्मी के पूजन में होता है। वह अपने भक्त को अक्षय सम्पत्ति अर्थात् दैवी सम्पदा प्रदान करती है। लक्ष्मी ब्रह्म का सम्पत्ति-प्रदायक स्वरूप है। वह स्वयं पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। इस प्रकार इस दिव्य त्रि-दिवसीय द्वितीय चरण में लक्ष्मी-पूजन सम्पन्न किया जाता है।
सरस्वती-पूजन
सर्वोच्च ज्ञान का उदय
दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन तथा विशुद्ध, सात्त्विक एवं दिव्य गुणों के विकास में सफलता प्राप्त करने के पश्चात् साधक एक अधिकारी व्यक्ति हो जाता है। इस स्थिति में वह परा ज्ञान के प्रकाश की सम्प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाता है। अब वह दिव्य ज्ञान की उपलब्धि के लिए स्वयं को सक्षम पाता है। इस चरण के अन्तर्गत देवी सरस्वती (जो दिव्य ज्ञान की साकार अभिव्यक्ति और ब्रह्मज्ञान का मूर्त रूप है) का श्रद्धापूर्ण पूजन किया जाता है। उसकी दिव्य वीणा से भव्य महावाक्य एवं प्रणव के उदात्त स्तर निःसृत होते हैं। वह अपने दिव्य नाद के ज्ञान-दान के पश्चात् अपने उज्वल एवं तुहिनवत् श्वेत वस्त्र के अनुरूप पूर्ण आत्म-ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार ज्ञानदात्री देवी सरस्वती के तुष्टिकरण के साथ इस तृतीय चरण का समापन होता।
दशवाँ दिन अर्थात् विजयादशमी देवी सरस्वती की कृपा के ज्ञान के अवतरण द्वारा प्राप्त जीवन्मुक्ति के उपलक्ष्य में व्यक्त विजयोल्लास का द्योतक है। अब जीव (सच्विदानन्द के) विशुद्धतम आत्म-भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह दिन अपनी लक्ष्य-सिद्धि या विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सुदूर आकाश में मानो विजयकेतु फहराने लगता है। इस अवसर पर साधक के कण्ठ से ये स्वर स्वतः फूट पड़ते हैं-"मैं 'वह' हूँ। मैं 'वह' हूँ; चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्, शिवोऽहम्; चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्, शिवोऽहम्।"
आध्यात्मिक सफलता को सुनिश्चित करने वाला एक संयोजन
साधक के आध्यात्मिक विकास में इस संयोजन की भी एक विशिष्ट अर्थवत्ता है। यह प्रत्येक साधक के विकास के अपरिहार्य चरणों का द्योतक है। इन चरणों से होते हुए आध्यात्मिक क्रम-विकास की यात्रा करना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। हम एक सोपान के पश्चात् दूसरे सोपान पर आरूढ़ होते हैं; किन्तु यदि हम प्रथम सोपान के पश्चात् अपनी साधना की यात्रा को लघुपथित करने के लिए अगले सोपानों की उपेक्षा कर देते हैं, तो परिणाम निश्चित रूप से दुःखद होते हैं। आजकल अनेक अज्ञ साधक आत्म-शुद्धि तथा दैवी सम्पत् की सम्प्राप्ति जैसी प्रारम्भिक पूर्वापेक्षाओं की पूर्ति के बिना ही पूर्ण आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के लिए आतुर हो उठते हैं। तत्पश्चात् यही लोग इस बात का उलाहना देते हैं कि साधना-पथ पर उनकी वांछित प्रगति नहीं हो रही है। उनकी यह प्रगति कैसे सम्भव हो सकती है? जब तक अशुद्धताओं का परिमार्जन एवं निष्कलुषता का विकास नहीं हो जाता, तब तक ज्ञान का अवतरण असम्भव है। अपवित्र भूमि पर सात्त्विकता के पौधे का विकास नहीं हो सकता।
इस संयोजन या व्यवस्था के अनुरूप आचरण करने से आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। यह आपका एकमात्र मार्ग है। मुक्ति के लिए इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ है। दुर्गुणों को नष्ट करके इनके स्थान पर स्वयं में इनके प्रतिपक्षी सद्गुणों को विकसित कीजिए। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको उस पूर्णत्व की उपलब्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप आप ब्रह्म से अभिन्न हो जायेंगे। आपके जीवन का परम उद्देश्य यही है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप आप समस्त ज्ञान-भण्डार के स्वामी हो जायेंगे। आप अपनी सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमत्ता को अनुभव करने लगेंगे। आप सभी वस्तुओं एवं व्यक्तियों में स्वयं को ही पाने लगेंगे। आप जीवन्मुक्त हो जायेंगे। आप जन्म-मरण के चक्र तथा संसार-रूपी दानव पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब आप सांसारिक क्लेशों तथा जन्म-मरण से सर्वथा असम्पृक्त हो जायेंगे। विजयश्री आपका वरण करेगी।
दिव्य माता की जय हो! वह आपको क्रमिक रूप से आध्यात्मिक सोपान के उच्चतम शिखर पर प्रतिष्ठित करके परमात्मा से एकीकृत करे!
सप्तम अध्याय
हिन्दू-उपासना
उपासना
उपासना ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह ईश्वर से सायुज्य की तीव्र लालसा और उससे हार्दिक तदाकारिता की आध्यात्मिक पिपासा की द्योतक है। भक्त भगवान् से उसके प्रति उत्कट भक्ति की सम्प्राप्ति तथा अज्ञानावरण के अपनयन के लिए प्रार्थना करता है। वह उसके सौम्य अनुग्रह के लिए लालायित रहता है। वह उसके निरन्तर नाम-स्मरण, उसके मन्त्रों के जप, उसके गुणगान तथा उसके कीर्तन में संलग्न रहता और उसकी लीलाओं का श्रवण तथा गायन करता है। वह उसके भक्तों की सुसंगति में उसके धाम में निवास करता है। वह उसके रूप, उसकी प्रकृति, उसके गुणों और उसकी लीलाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किये रहता है। वह अपने नेत्रों को बन्द करके प्रभु के स्वरूप का मानस-दर्शन करता है तथा परम शान्ति और चरम आनन्द का उपभोग करता है।
उपासना ईश्वर की उपस्थिति में रहने अथवा उसके सान्निध्य में पहुँचने के लिए किया गया उपासक का प्रयास है। 'उपासना' का शाब्दिक अर्थ है-ईश्वर के निकटस्थ होना। शास्त्रों तथा गुरु द्वारा उपदिष्ट विधि से अपने अभीप्सित आदर्श या उपास्य देवता पर अपना ध्यान केन्द्रित करके उनकी ओर अग्रसर होने को उपासना कहा जाता है। एक पात्र से अन्य पात्र में तेल डालते समय गिरते हुए तेल में जो प्रत्ययैकतानता होती है, वही प्रत्ययैकतानता उपासक के विचार में भी होनी चाहिए। इसे तैलधारावत् होना चाहिए। इसमें वे सभी शारीरिक तथा मानसिक अनुपालन एवं अभ्यास सन्निहित हैं जिनके द्वारा जिज्ञासु आध्यात्मिकता के क्षेत्र में संयमित और सन्तुलित प्रगति करता है और अन्ततः उसे अपने हृदय में ईश्वरत्व की विद्यमानता की प्रतीति होने लगती है।
उपासना की उपलब्धियाँ
प्रभु की उपासना से उपासक को हृदय की शुद्धि, आध्यात्मिक स्पन्दनों की समस्वरता, मन की सुस्थिरता, संवेगों के परिमार्जन तथा परिष्कार, पंचकोषों के समुचित समायोजन और अन्ततः ईश्वर-साक्षात्कार या ब्रह्मात्मभाव की सम्प्राति होती है।
उपासना से भक्त ईश्वर के निकट हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे प्रभु से संलाप करने की क्षमता भी प्राप्त हो जाती है और उसका मन शुद्ध भाव तथा ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम से आप्लावित हो उठता है। यह मनुष्य को शनैः शनैः दिव्य रूप में रूपान्तरित कर देती है।
उपासना से मनस्तत्त्व में परिवर्तन और रजस् तथा तमस् का निराकरण हो जाता है। फलस्वरूप, मन सात्त्विकता से ओत-प्रोत हो जाता है। इससे वासना, तृष्णा, अहंकार, काम, घृणा, क्रोधादि का भी क्षय होता है। उपासना उपासक की अन्तर्मुखी वृत्ति को जाग्रत कर देती है। अन्ततः उसके माध्यम से वह ईश्वर का सायुज्य प्राप्त कर जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उपासना उसे अमरत्व तथा मुक्ति प्रदान करती है।
भ्रमर-कीट-न्याय के अनुसार मन अपने ध्येय विषय के साथ तद्रूप हो जाता है। आपकी प्रकृति आपके विचारों के अनुरूप ही होती है- यह एक अपरिवर्तनीय मनोवैज्ञानिक सत्य है। उपासना में एक ऐसी रहस्यात्मक अचिन्त्य शक्ति निहित है जो ध्याता तथा ध्येय को परस्पर अभिन्न कर देती है।
भगवद्गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं-"हे परन्तप अर्जुन, मेरी अनन्य भक्ति से ही मेरा दर्शन, मेरा ज्ञान तथा मुझमें पूर्णतः अनुस्यूत हो जाना सम्भव है" (११/५४)।
महर्षि पतंजलि ने उपासना के महत्त्व पर अपने राजयोग-सूत्रों में कई स्थलों पर पर्याप्त बल दिया है, क्योंकि उपासना राजयोगी के लिए भी आवश्यक है। राजयोगी का एक अपना पथ-प्रदर्शक इष्टदेवता होता है—वह चाहे योगेश्वर कृष्ण हों या योगीश्वर शंकर भगवान्। ईश्वर-प्रणिधान राजयोग और क्रियायोग का एक अंग है। पतंजलि कहते हैं-"उपासना से मनुष्य समाधिस्थ हो सकता है।"
आत्मिक उन्नयन, आध्यात्मिक प्रगति तथा जीवन को धर्मोन्मुख बनाने के लिए जिन उत्प्रेरक उपकरणों की आवश्यकता होती है, उनमें उपासना मात्र एक अनिवार्य आवश्यकता ही नहीं, अपितु समाज के प्रत्येक वर्ग तथा श्रेणी के लिए लाभप्रद भी है। इसका साधन भी सरल है।
जहाँ तक पशु तथा मानव के परस्पर सम्बन्ध का प्रश्न है-भोजन, पान, निद्रा, भय, मैथुनादि उभयनिष्ठ हैं। जो वस्तु मनुष्य को यथार्थ मानव या धर्माभिमुख बनाती है, वह है धार्मिक चेतना। जिस मनुष्य का जीवन केवल बहिर्मुखी तथा वासनाग्रस्त है एवं जो किसी प्रकार की उपासना नहीं करता, वह बाह्यतः मानव शरीर-धारी होते हुए, भी यथार्थतः पशु ही है।
सगुणोपासना तथा निर्गुणोपासना
प्रतीक-उपासना तथा अहंग्रह-उपासना- ये उपासना के दो प्रकार हैं। प्रतीक-उपासना सगुणोपासना है, जब कि अहंग्रह-उपासना निर्गुणोपासना है जिसमें निराकार तथा निर्गुण अक्षर या परात्पर ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। शालग्राम, मूर्ति तथा भगवान् राम, भगवान् कृष्ण, गायत्री देवी आदि के चित्रों पर ध्यान केन्द्रित करना प्रतीक-उपासना है। विस्तृत नील वर्ण आकाश, सर्वव्यापी वायु तथा सूर्य का सर्वव्यापी तेज अमूर्त-उपासना के प्रतीक हैं। सगुणोपासना मूर्त तथा निर्गुणोपासना अमूर्त-उपासना है।
भगवान् कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन या उनके नामों का गुणगान, प्रभु का अनवरत स्मरण, उनका पाद-सेवन, माल्यार्पण, वन्दन, प्रार्थना, मन्त्रोच्चारण, आत्मसमर्पण एवं भगवद्भक्तों, मानवता तथा देश की नारायण-भाव से सेवा सगुणोपासना के अवयव हैं।
आत्म-भाव से ॐ का गायन, आत्म-भाव से मानवता तथा देश की सेवा, आत्म-भाव या ब्रह्म-भाव से ॐ का मानसिक जप, 'सोऽहम्' या 'शिवोऽहम्' का ध्यान या 'नेति-नेति' सिद्धान्त द्वारा मायिक चक्र को निरस्त कर 'अहं ब्रह्मास्मि' या 'तत्त्वमसि' जैसे महावाक्यों पर ध्यान केन्द्रित करना अहंग्रह-उपासना या निर्गुणोपासना है।
सगुणोपासना भक्तियोग तथा निर्गुणोपासना ज्ञानयोग है। सगुण (सविशेष) ब्रह्म तथा निर्गुण (निर्विशेष) ब्रह्म के उपासकों को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है; परन्तु भक्तियोग की अपेक्षा ज्ञानयोग अधिक दुष्कर है, क्योंकि इस आध्यात्मिक साधना के प्रारम्भ में ही देहाभिमान का परित्याग कर देना पड़ता है। जिनमें देहाभिमान है, उनके लिए अक्षर या अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति अत्यधिक कठिन है। इसके अतिरिक्त निराकार तथा निर्गुण ब्रह्म पर मन को स्थिर करना अत्यन्त दुःसाध्य है। अक्षर या निर्गुण ब्रह्म की धारणा के लिए सुतीक्ष्ण, एकाग्र तथा सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है।
भक्तियोग में भाव
भक्तियोग ज्ञानयोग या आध्यात्मिक ध्यान की अपेक्षा अधिक सरल है। भक्तियोग में भक्त प्रभु के साथ निकट एवं प्रेमपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके धीरे-धीर अपनी प्रकृति, रुचि तथा क्षमता के अनुसार भक्ति के छह भावों में से किसी एक भाव की साधना करता है।
शान्त-भाव, दास्य-भाव, सख्य-भाव, वात्सल्य-भाव, कान्ता-भाव और माधुर्य-भाव भक्त के षड्लक्षण या भगवान् के प्रति उसके छह भाव हैं। प्रकार-भेद तथा भावनात्मक तीव्रता के वैभिन्य के कारण भाव परस्पर भिन्न होते हैं। इन भिन्न-भिन्न भावों का वर्गीकरण इनकी तीव्रता के अनुरूप होता है। शिशु की माता-पिता के प्रति जो भावना होती है, वही भावना भगवान् के प्रति प्रह्लाद तथा ध्रुव की थी। यह शान्त-भाव है। दास्य-भाव में भक्त का आचरण एक दास की भाँति होता है। उसका भगवान् ही उसका स्वामी होता है। हनुमान् भगवान् के आदर्श दास है। सख्य-भाव में समानता की भावना होती है। अर्जुन और कुचेला में यही भाव था। वात्सल्य-भाव में भक्त भगवान् को शिशुवत् समझता है। यशोदा तथा कौसल्या में क्रमशः श्रीकृष्ण तथा श्रीराम के प्रति यही भाव था। पति के प्रति पत्नी का जो भाव होता है, उसे कान्ता-भाव कहते हैं। सीता और रुक्मिणी में यही भाव था। माधुर्य-भाव इन समस्त भावों की पराकाष्ठा है। इसमें प्रेम की तीव्रता के कारण प्रेमी-प्रेमिका एक हो जाते हैं। राधा और मीरा में इसी प्रकार का भाव था।
माधुर्य-भाव भक्ति का चरमोत्कर्ष है। इसमें भगवान् में भक्त का अन्तर्लयन हो जाता है। इस भाव को प्राप्त भक्त भगवान् की आराधना, उसका निरन्तर स्मरण, उसका कीर्तन, उसकी महिमा का वर्णन, उसके नाम की आवृत्ति, उसका मन्त्रोच्चारण, उसकी प्रार्थना एवं उसको दण्डवत् प्रणाम करता है। वह उसकी लीलाओं का श्रवण, उसके प्रति अप्रतिबन्धित तथा उन्मुक्त भाव से आत्मसमर्पण करता और उसी कृपा तथा उसका सान्निध्य प्राप्त करके अन्ततः उसमें अन्तर्लीन हो जाता है।
माधुर्य-भाव में भक्त तथा भगवान् का निकटतम सम्बन्ध होता है। कान्ता-भाव तथा माधुर्य-भाव में विषयासक्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता। ये भाव कामुकता से पूर्णतः असम्पृक्त होते हैं। कामुक या दूषित भाव-प्रवण लोगों के लिए इन दो भावों का ज्ञान असम्भव है; क्योंकि इनके मन में दूषित भावनाएँ या निरन्तर कामुक प्रवृत्तियाँ बद्धमूल हो चुकी होती हैं। सूफी सन्तों में भी प्रेमी-प्रेमिका का माधुर्य-भाव होता है। जयदेव-रचित गीतगोविन्द माधुर्य-रस से पूर्ण है। रहस्यवादियों द्वारा प्रयुक्त प्रेम की भाषा का अर्थ ठीक-ठीक समझना सांसारिक व्यक्तियों के लिए असम्भव है। इस भाषा का ज्ञान केवल गोपियों, राधा, मीरा, तुकाराम, नारद, हाफिज़ तथा उनके जैसे अन्य महान् भगवद्-भक्तों के लिए ही सम्भव है।
पूजा तथा इष्टदेवता
पूजा वैधी उपासना के लिए प्रयुक्त एक सामान्य पारिभाषिक शब्द है। इसके लिए अर्चन, वन्दन, भजनादि जैसे अनेक समानार्थक शब्दों का व्यवहार किया जाता है; किन्तु ये शब्द पूजा के कुछ निश्चित पक्षों के द्योतक हैं। भक्त का इष्टदेवता या देवता का कोई विशिष्ट रूप पूजा का विषय होता है। वैष्णवों के लिए नारायण या विष्णु या राम या कृष्ण के रूप में उनके विग्रह, शैवों के लिए शिव के अष्ट-रूप तथा शाक्तों के लिए देवी उपास्य हैं।
कभी-कभी भक्त पूजा के लिए अपने कुलदेवता या कुलदेवी का चयन कर लेता है और कभी-कभी देवता का चुनाव उसके गुरु द्वारा होता है। किन्हीं अवसरों पर वह स्वयं ऐसे देवता का चयन कर लेता है जो उसकी भावनाओं को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। वही उसके इष्टदेवता होते हैं।
बाह्य पूजा में किसी प्रतिमा, किसी चित्र या किसी प्रतीक जैसे विषय या आलम्बन को प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ विष्णु-पूजा के लिए शालग्राम तथा शिव-पूजा के लिए लिंग का प्रयोग किया जाता है।
पूजा का विषय सभी वस्तुएँ हो सकती हैं; किन्तु स्वभावतः इसके लिए उन्हीं वस्तुओं का चुनाव किया जाता है जो उपासक के मन को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। प्रतिमा या उपयोगी प्रतीक भक्त के मन में देवता के विचार को जाग्रत कर सकता है। शालग्राम-शिला मन की एकाग्रता को सरलतापूर्वक जाग्रत कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में किसी प्रतीक या प्रतिमा के प्रति अनुराग होता है। मूर्ति (विग्रह), सूर्य, अग्नि, जल, गंगा, शालग्राम तथा लिंग-ये सब परमात्मा के प्रतीक हैं जो साधकों के मन की एकाग्रता और हृदय की शुद्धि के लिए उपयोगी हैं। प्रतिमाओं या प्रतीकों की विशेष क्षमता के प्रति अपनी-अपनी आस्था के कारण उपासकों का व्यक्तिगत स्तर पर उनकी और रुझान हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि मन किसी विशेष प्रतीक या प्रतिमा के माध्यम से इच्छित दिशा में ही सुचार रूप से कार्य करता है।
मानवता के अधिकांश का मन या तो अपवित्र है या दुर्बल। अतः इन लोगों की उपासना का विषय अनिवार्य रूप से पवित्र होना चाहिए। जो विषय वासना तथा घृणा की मनोवृत्तियों के लिए उत्तेजक होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए; किन्तु कोई उन्नत भक्त जिसका मन विशुद्ध है और जो प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक वस्तु में दिव्य सत्ता का दर्शन करता है, किसी भी वस्तु की उपासना कर सकता है।
पूजा में किसी दिव्य रूप का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिमा या चित्र को उपास्य विषय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रतिमा की आराधना की जाती है। प्रतिमा, शिला या विग्रह या मूर्ति-ये सभी आलम्बन किसी ऐसे देवता-विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका इनमें आवाहन किया जाता है। लिंग शिव का प्रतिनिधित्व करता है। यह अद्वितीय तथा निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। श्रुति में आया है : "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म-एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है।" यहाँ द्वैत नहीं है। लिंग नेत्रों के लिए उज्ज्वल तथा आकर्षक एवं मन की एकाग्रता के लिए उपयोगी है।
शालग्राम विष्णु की प्रतिमा तथा उसका प्रतीक है। भक्त विशेष की अभिरुचि के अनुसार श्रीराम, श्रीकृष्ण, कार्तिकेय, गणेश, हनुमान्, दत्तात्रेय, सीता, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली, सरस्वती आदि की प्रतिमाओं का विधान है।
विष्णु तथा उनके अवतारों एवं शक्ति एवं शिव की प्रतिमाएँ ऐसी लोकप्रिय हैं जिनका पूजन मन्दिरों तथा घरों-दोनों स्थानों पर होता है। तिरुपति, पण्ढरपुर, पलनि तथा कतिरगाम आदि मन्दिरों के विग्रह शक्तिमान् देवता हैं। वे प्रत्यक्ष देवता हैं। वे भक्तों को वरदान देते, रोगमुक्त करते और उन्हें दर्शन देते हैं। इन देवताओं की लीलाएँ अद्भुत हैं। हिन्दू-धर्म बहुदेववादी नहीं है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा तथा शक्ति एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप हैं।
परमात्मा अपने भक्तों के समक्ष स्वयं को विभिन्न रूपों में अनावृत करता है। वह वही रूप ग्रहण करता है जिसका चयन भक्त अपनी उपासना के लिए किये रहता है। यदि आप उसकी पूजा चतुर्भुज हरि के रूप में करते हैं, तो वह आपके समक्ष हरि के रूप में प्रकट होगा और यदि आप उसकी पूजा शिव के रूप में करते हैं, तो वह आपको शिव के रूप में दर्शन देगा। यदि आप उसकी पूजा माँ दुर्गा या काली के रूप में करते हैं, तो वह आपके सम्मुख दुर्गा या काली के रूप में प्रकट होगा, यदि आप उसकी पूजा भगवान् राम, भगवान् कृष्ण या भगवान् दत्तात्रेय के रूप में करते हैं, तो वह आपके निकट राम, कृष्ण या दत्तात्रेय के रूप में उपस्थित होगा और यदि आप उसकी पूजा ईसा या अल्लाह के रूप में करते हैं, तो वह आपके समक्ष ईसा या अल्लाह के रूप में प्रकट होगा।
शिव या हरि, गणेश या सुब्रह्मण्य या दत्तात्रेय या भगवान् का कोई भी अवतार, राम या कृष्ण, सरस्वती या लक्ष्मी, गायत्री या काली, दुर्गा या चण्डी-इनमें से आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। ये सब एक ही ईश्वर के रूप हैं। उपास्य का कोई भी नाम और रूप हो-उपासना ईश्वर की ही होती है। अन्तर्व्यापी ईश्वर ही अपने विग्रह में अधिष्ठित हो कर पूजा ग्रहण करता है। यह नितान्त भ्रान्त धारण है कि एक रूप किसी अन्य रूप से श्रेष्ठतर है। सभी रूप एक तथा समतुल्य हैं। शिव, विष्णु, गायत्री, राम, कृष्ण, देवी तथा ब्रह्म एक ही हैं। एक ही ईश्वर हम सबका उपास्य है। जो विभिन्नता दृष्टिगत होती है, उसका कारण उपास्य विग्रहों की परस्पर विभिन्नता न हो कर उपासकों की परस्पर विभिन्नता है। अज्ञान के कारण ही विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों के अनुयायी परस्पर संघरर्षरत रहते हैं।
मूर्ति-पूजा का दर्शन तथा महत्त्व
मूर्ति-नवदीक्षित आध्यात्मिक साधकों का आलम्बन
मूर्ति नवदीक्षितों के लिए एक आलम्बन है। यह उनके आध्यात्मिक शैशव का आश्रय-स्थान है। प्रारम्भ में उपासना के लिए कोई रूप या प्रतिमा आवश्यक होती है। उपासना के लिए यह परमात्मा का एक बाह्य प्रतीक है। यह परमात्मा का स्मरण कराती है। भौतिक प्रतिमा मानसिक विचार को उत्प्रेरित करती है। मूर्ति-पूजा से मन सुस्थिर तथा सन्तुलित होता है। उपासक के लिए असीमता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, विशुद्धता, पूर्णत्व, स्वातन्त्र्य, पावनता, सत्य तथा सर्वव्यापकता की अवधारणाओं से संयुक्त होना अनिवार्य है। असीम या निरपेक्ष सत्ता पर ध्यान केन्द्रित कर पाना सबके लिए सम्भव नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए एकाग्रता के अभ्यास हेतु मूर्त रूप आवश्यक है। सर्वत्र परमात्मा का दर्शन और उसकी उपस्थिति का भान सामान्य जन के लिए असम्भव है। आधुनिक मनुष्य के लिए मूर्ति-पूजा उपासना की सरलतम विधि है।
मन की स्थिरता के लिए किसी प्रतीक की अनिवार्यता असन्दिग्ध है। आश्रय के लिए मन को एक आलम्बन की आवश्यकता होती है। प्रारम्भिक चरणों में मन में चरम सत्ता की अवधारणा असम्भव होती है। उक्त अवस्था में किसी बाहा सहयोग के अभाव में मन का केन्द्रीभूत होना सम्भव नहीं हो पाता। प्रारम्भ में बिना किसी प्रतीय के मन को एकाग्र या ध्यानमन कर पाना असम्भव होता है।
प्रत्येक व्यक्ति मूर्तिपूजक है
वेदों में मूर्ति-पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता; किन्तु पुराणों तथा आगमों में घरों तथा मन्दिरों-दोनों में मूर्ति-पूजा का विवरण मिलता है। मूर्ति-पूजा का प्रवलर केवल हिन्दू-धर्म में है, ऐसी बात नहीं है। ईसाई क्रास को पूजते हैं। उनके मन में क्राए की प्रतिमा अधिष्ठित रहती है। मुसलमान जब विनत हो कर नमाज अदा करते हैं, तथ उनकी मानसिकता में काबा का पत्थर रचा-पचा रहता है। कुछ योगियों तथा वेदान्तियों के अतिरिक्त संसार के सभी लोग मूर्तिपूजक हैं। उनके मन में किसी-न-किसी प्रतिमा के लिए स्थान अवश्य होता है।
मानसिक प्रतिमा भी मूर्ति का ही रूप है। इन दोनों में प्रकार-भेद न हो का केवल मात्रा-भेद है। सभी उपासक, वे कितने ही प्रतिभा सम्पन्न क्यों न हों, अपने मन में किसी रूप को प्रतिष्ठित करके उस पर अपने मन को स्थिर करते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति मूर्तिपूजक होता है। चित्र या रेखांकन आदि प्रतिमा या मूर्ति के ही रूप हैं। स्थूल बुद्धि वाले व्यक्ति के आलम्बन के लिए मूर्त प्रतीक तथा सूक्ष्म बुद्धि वाले व्यक्ति के आलम्बन के लिए अमूर्त प्रतीक अपेक्षित होते हैं। वेदान्ती भी चंचल मन की स्थिरता के लिए ॐ को प्रतीक-रूप में प्रयुक्त करता है। केवल चित्रों अथवा पाषाण या काष्ठ की प्रतिमाओं को ही मूर्ति नहीं कहा जाता, मनीषी तथा नेता भी मूर्तिवत् उपास्य हो जाते हैं। तब मूर्ति-पूजा की निन्दा क्यों ?
ईश्वर से सम्पर्क-स्थापन का माध्यम
मूर्ति मूर्तिकार की अर्थहीन कल्पना न हो कर एक ऐसा देदीप्यमान माध्यम है जो भक्त को आकर्षित करके उसे ईश्वरोन्मुख कर देता है। प्रतिमा-पूजन के साथ-साथ भक्त के हृदय में प्रभु की उपस्थिति की अनुभूति होने लगती है और उसका भक्ति-भाव उमड़ कर प्रभु की ओर प्रवाहित होने लगता है। आधुनिक विषयासक्त मानव के अज्ञान के कारण उसकी दृष्टि आच्छादित हो जाती है और वह परमात्मा के स्वरूप की प्रिय तथा सम्मोहक मूर्ति में प्रतिष्ठित दिव्य सत्ता का दर्शन नहीं कर पाता। इस शताब्दी की वैज्ञानिक प्रगति से ही आपको मूर्ति-पूजा की महिमा के सम्बन्ध में आश्वस्त हो जाना चाहिए। रेडियो नामक एक लघु पेटिका गायकों तथा वक्ताओं को किस प्रकार अपने में तल्लीन बनाये रखती है! यह एक यान्त्रिक तथा निर्जीव संरचना मात्र है जो तीव्र गति से फेंके जाने पर सहस्र खण्डों में विभाजित हो सकता है; किन्तु यदि आप इसके उपयोग करने की विधि से परिचित हैं तो आप इसके माध्यम से सहस्रों मील दूर गाये जाने वाले संगीत तथा विश्व के सुदूर स्थानों में होने वाले भाषणों का आनन्द उठा सकते हैं। जिस प्रकार रेडियो द्वारा आप समस्त विश्व के लोगों की ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार आपके लिए एक मूर्ति के माध्यम से सर्वव्यापी परमात्मा से सम्पर्क स्थापित करना भी सम्भव है। सर्वव्यापी परमात्मा की दिव्यता का स्पन्दन सृष्टि के कण-कण में हो रहा है। क्या दिक्काल का कोई ऐसा अणुवत् स्थान भी है जहाँ वह विद्यमान न हो। तब आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह मूर्ति में विद्यमान नहीं है?
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहज ही कह देंगे- "ईश्वर तो एक सर्वव्यापी निराकार सत्ता है। उसे एक मूर्ति में कैसे आबद्ध किया जा सकता है?" क्या इन लोगों को कभी उसकी सर्वव्यापकता का ज्ञान हो पाता है? क्या ये लोग उसे केवल उसे-प्रत्येक वस्तु में सर्वदा परिव्याप्त देख पाते हैं? इसका एकमात्र उत्तर है नहीं। यह उनका केवल अहंकार है जो उन्हें ईश्वर की प्रतिमा के सम्मुख विनत नहीं होने देता है और इसी कारण वे अपना अर्थहीन तर्क प्रस्तुत कर देते हैं।
"अधजल गगरी छलकत जाय।" आध्यात्मिक दृष्टि से एक व्यवहार-कुशल व्यक्ति, जो ध्यान तथा उपासना में संलग्न रहता है और जिसका हृदय ज्ञान तथा अकृत्रिम भक्ति से ओत-प्रोत रहता है, वह सर्वदा मौन रहता है। वह मौन के माध्यम से ही अन्य लोगों को प्रभावित और प्रशिक्षित किया करता है। केवल वही इस तथ्य से अवगत हो सकता है कि मानसिक एकाग्रता के लिए प्रारम्भ में किसी मूर्ति की आवश्यकता होती है या नहीं।
किसी की बुद्धि कितनी भी कुशाग्र क्यों न हो, वह किसी प्रतीक के अभाव में अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता। एक प्रतिभा सम्पन्न या विद्वान् व्यक्ति ही अपने अहंकार तथा दम्भ के कारण कहता है- "मुझे मूर्ति पसन्द नहीं है। मैं किसी रूप पर अपने मन को स्थिर करना नहीं चाहता।" वस्तुतः उसके लिए किसी निराकार सत्ता पर भी मन को एकाग्र कर पाना असम्भव होता है। वह सोचता है कि यदि लोगों को यह ज्ञात हो जायेगा कि वह साकार या सगुण सत्ता की उपासना करता है, तो वह उनके उपहास का पात्र हो जायेगा। वास्तविकता तो यह है कि वह किसी निर्गुण-निराकार सत्ता की भी उपासना नहीं करता। वह केवल बातें बनाता है और बहस करता तथा ढोंग रचता है। केवल अनावश्यक वाद-विवाद में ही उसके समय का अपव्यय होता है। अनेक सिद्धान्तों की अपेक्षा एक अभ्यास श्रेष्ठतर है। अधिकांश बुद्धिवादियों की बुद्धि उनके मार्ग में अवरोध ही उपस्थित करती है। ये लोग ब्रह्म की सत्ता को अनुमान-जन्य, समाधि को मन की प्रतारणा तथा आत्मसाक्षात्कार को वेदान्तियों की कल्पना मात्र मानते हैं। कितने मोहग्रस्त हैं वे। वे अज्ञान के आवरण में आबद्ध हो कर अपनी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता-जो आत्मज्ञान की तुलना में नितान्त नगण्य है-से दिग्भ्रमित हो गये हैं। इस प्रकार के लोगों की मुक्ति के लिए कोई आशा नहीं। सर्वप्रथम शुभ संस्कारों द्वारा उनके अशुभ संस्कारों का परिमार्जन किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात् ही वे अपनी त्रुटियों को समझ सकेंगे। परमात्मा उनकी बुद्धि को निर्मल करके यथार्थ ज्ञान के प्रति उनमें जिज्ञासा जाग्रत करे!
परमात्मा का एक प्रतीक
प्रतिमा (मूर्ति) एक प्रतीक है। मन्दिर में प्रतिष्ठित मूर्ति पत्थर, लकड़ी या धातु से निर्मित की जाती है; किन्तु भक्त के लिए यह एक बहुमूल्य वस्तु है। इसका कारण है कि इसमें भगवान् का चिह्नांकन है और यह उसकी प्रतीक है जिसे वह पवित्र और शाश्वत समझता है। ध्वज एक चित्रांकित वस्त्र का अंश मात्र होता है; किन्तु वह एक सैनिक के लिए उस वस्तु का प्रतीक है जो उसके लिए अत्यधिक प्रिय है। वह इस ध्वज के रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग के लिए भी उद्यत रहता है। इसी प्रकार भक्त के लिए प्रतिमा भी अत्यन्त प्रिय होती है। वह भक्त से अपनी भक्ति की भाषा में वार्तालाप करती है। जिस प्रकार ध्वज सैनिक में सामरिक शौर्य जाग्रत करता है, उसी प्रकार प्रतिमा भक्त में भक्ति-भाव जाग्रत करती है। प्रतिमा में ईश्वर का अध्यारोपण हुआ रहता है और इससे उपासक में दैवी विचारों की सृष्टि होती है।
कागज का कोई टुकड़ा मूल्यहीन होता है। आप उसे फेंक दिया करते हैं; किन्तु जब उस पर राजकीय चिह्न अंकित कर दिया जाता है अर्थात् जब वह कोई करेंसी नोट बना दिया जाता है, तब आप उसे अपने बटुवे या बक्स में सुरक्षित रख देते हैं। इसी प्रकार आपके लिए किसी सामान्य शिलाखण्ड का कोई मूल्य नहीं होता। आप उसकी उपेक्षा कर देते हैं। किन्तु यदि आप पण्ढरपुर में भगवान् कृष्ण की प्रस्तर-प्रतिमा या किसी अन्य मन्दिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा का दर्शन करते हैं, तो आप करबद्ध हो कर उसके सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उस प्रस्तर पर प्रभु का चिह्न अंकित है। भक्त प्रस्तर-प्रतिमा पर अपने आराध्य प्रभु को उनके समस्त गुणों के साथ अध्यारोपित कर देता है।
मूर्ति-पूजन के समय आप यह नहीं कहते कि यह अमुक स्थान से आयी है, अमुक ने भेजी है, यह अमुक वस्तु से निर्मित है, यह अमुक मूल्य दे कर खरीदी गयी है आदि। आप उस प्रतिमा में प्रभु के समस्त गुणों का अध्यारोपण कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं-"हे अन्तर्यामी ! तुम सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ तथा दयामय हो। तुम सर्वभूतों के आदि स्रोत, स्वयम्भू, सत्-चित्-आनन्द, नित्य तथा अविकारी हो। तुम मेरे जीवन के जीवन और मेरी आत्मा की आत्मा हो। मुझे प्रकाश और ज्ञान दो। तुम सर्वदा के लिए मेरा आश्रय-स्थल बन जाओ।" जब आपकी भक्ति तथा ज्ञान में तीव्रता एवं गहनता का प्रवेश हो जाता है, तब आपको प्रस्तर-प्रतिमा का दर्शन नहीं होता। उसमें आप उस प्रभु का ही दर्शन करते हैं जो चैतन्य है। नव-साधकों के लिए मूर्ति-पूजा अत्यावश्यक है।
विराट् का अविकल अंग
नव-साधक की साधना के प्रारम्भिक चरण में प्रतिमा नितान्त आवश्यक है। प्रतिमा-पूजन से ईश्वर प्रसन्न होता है। प्रतिमा पाँच तत्त्वों से निर्मित होती है। ईश्वर का शरीर भी पाँच तत्त्वों से निर्मित होता है। प्रतिमा तो प्रतिमा ही रह जाती है; किन्तु पूजा ईश्वर तक पहुँच जाती है।
जब आप किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, तब वह बहुत प्रसन्न होता है। आप उसके शरीर के अल्पांश का ही स्पर्श कर रहे होते हैं; किन्तु इतने से ही उसे आनन्द प्राप्त हो जाता है। वह मुस्करा कर आपका स्वागत करता है। इसी प्रकार ईश्वर भी अपने विराट् शरीर के अल्पांश के पूजन से अत्यन्त प्रसन्न होता है। मूर्ति भगवान् के शरीर का एक अंग है। अखिल विश्व उसका शरीर है, उसका विराट् रूप है। पूजा भगवान् तक पहुँच जाती है। उपासक प्रतिमा में भगवान् तथा उसके समस्त गुणों को अध्यारोपित कर देता है। वह मूर्ति के माध्यम से भगवान् की सोलह प्रकार की सेवा अर्थात् षोडशोपचार करता है। पहले उसकी उपस्थिति के लिए उसका आवाहन करता है। इसके पश्चात् उसे आसन प्रदान किया जाता है। फिर उसका पाद-प्रक्षालन किया जाता है। तत्पश्चात् उसे अर्घ्य-दान दिया जाता है (अर्घ्य अतिथि-सत्कार का द्योतक है)। इसके पश्चात् स्नान कराया जाता है। फिर उसे वस्त्राभूषित किया जाता है। फिर यज्ञोपवीत किया जाता है। तत्पश्चात् उसको चन्दन लगाया जाता है। फिर उसे पुष्प अर्पित किये जाते हैं (ये श्रद्धा-सुमन भगवान् के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा के प्रतीक होते हैं)। फिर धूप जलायी जाती है। इसके बाद दीप जला कर उसकी आरती उतारी जाती है। तत्पश्चात् उसे नैवेद्य और फिर ताम्बूल अर्पित किये जाते हैं। इसके बार कर्पूर जला कर उसका नीराजन किया जाता है। इसके पश्चात् उसे स्वर्ण-पुष्य अभि किये जाते हैं। अन्त में देवता से विदा ली जाती है (विसर्जन)। पूजा के इन वादा रुभे मैं भक्त के आन्तरिक प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। उसका चंचल मन स्थिर हो जाता है। इससे साधक को क्रमशः ईश्वर के सामीप्य का बोध होने लगता है, उसका हदा विशुद्ध हो जाता है और धीरे-धीरे वह अपने अहंकार को नष्ट कर देता है। प्रतीक के प्रति आस्थावान् भक्त प्रस्तर, मृत्तिका और पीतल की मूर्ति, चित्र, शालग्राम आदिये भगवान् के शरीर का ही दर्शन करता है। इस प्रकार की उपासना मूर्ति-पूजा हो ही नहीं सकती। समस्त पदार्थ परमात्मा का प्रकटीकरण हैं। वह संसार की सभी वस्तुओं में विद्यमान है। प्रत्येक वस्तु उपासना का विषय है; क्योंकि परमात्मा स्वयं को प्रत्येक वस्तु में अभिव्यक्त करता है और उसमें अवस्थित हो कर पूजित होता है। उपासना के उपक्रम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जो पूजा का विषय है, वह वरिष्ठ एवं चेतन है। वस्तुओं के प्रति यह धारणा भक्त के लिए अत्यन्त आवश्यक है। वस्तुओं को देखने-परखने के उक्त दृष्टिकोण के लिए अप्रशिक्षित मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता आवश्यक है।
मूर्ति-पूजा से भक्ति का विकास
मूर्ति-पूजा मनुष्य की एकाग्रता को सरल तथा सहज बना देती है। आप परमात्मा को उसके किसी अवतार-विशेष के रूप में देखते हैं। मूर्ति-पूजा के माध्यम से आप अपने मनश्चक्षु से उक्त अवतार में अवस्थित परमात्मा की महान् लीलाओं को देख सकते हैं। इस विधि की गणना आत्मसाक्षात्कार की सरलतम विधियों में की जाती है।
जिस प्रकार किसी प्रख्यात योद्धा के चित्र से आपके मन में शौर्य की भावना जाग्रत होती है, उसी प्रकार ईश्वर का चित्र-दर्शन करने से मन दिव्यता के शिखर पर आरूढ़ हो जाता है। जिस प्रकार अपने खिलौने में किसी शिशु को अध्यारोपित करके उसके साथ खेलते हुए तथा उसे काल्पनिक स्तन-पान कराते हुए किसी शिशु में मातृ-भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार भक्त प्रतिमा की उपासना तथा उस पर अपना ध्यान केन्द्रित करके अपनी भक्ति-भावना को विकसित करता है ।
नियमित पूजा से प्रतिमा-स्थित देवत्व का अनावरण
नियमित पूजा तथा मूर्ति में निहित देवत्व के प्रति आस्था-जनित हमारी आन्तरिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली अन्य विधाओं से मूर्ति में अन्तर्निहित देवत्व अनावृत हो जाता है। निश्चित रूप से यह एक आश्चर्यजनक तथा चमत्कारपूर्ण तथ्य है कि प्रतिमा सजीव तथा मुखर हो कर आपके प्रश्नों के उत्तर तथा आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने लगती है। आपके अन्तर में परिव्याप्त परमात्मा मूर्ति में प्रसुप्त देवत्व को जाग्रत करने में सक्षम है। यह उस शक्तिशाली लेंस की भाँति है जो सूर्य की किरणों को कपास के ढेर पर केन्द्रीभूत कर देता है। लेंस और कपास दोनों में से कोई भी अग्नि नहीं है और सूर्य की किरणें भी कपास को स्वयं जला पाने में असमर्थ हैं। जब इन तीनों को एक विशिष्ट विधि से एकत्र कर दिया जाता है, तभी अग्नि उत्पन्न हो कर कपास को जला पाती है। प्रतिमा, साधक तथा सर्वव्यापी परमात्मा के सम्बन्ध में भी यही सिद्धान्त लागू होता है। पूजा प्रतिमा को दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर देती है और तब प्रभु उस प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यहाँ से ही वे एक विशिष्ट विधि से आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रतिमा से चमत्कार की सृष्टि होती है। जिस स्थान पर प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा होती है, वह तत्क्षण मन्दिर के रूप में परिणत हो जाता है। मन्दिर ही क्यों, वह स्थान तो वैकुण्ठ या कैलास ही हो जाता है। वहाँ कि निवासी दुःख-दैन्य, व्याधि, विफलता तथा स्वयं संसार से भी मुक्त हो जाते हैं। प्रतिमा में जाग्रत परमात्मा किसी अभिभावक देवदूत का उत्तरदायित्व बहन करता है और अपने सम्मुख श्रद्धा-विनत होने वालों के शीश पर आशिष-वर्षण करते हुए उन्हें आत्यन्तिक सुख प्रदान करता है।
प्रतिमा चिद्घन है
प्रतिमा दिव्य सत्ता का प्रतीक मात्र है। भक्त को उसमें किसी शिला-खण्ड या धातु-राशि के दर्शन नहीं होते। उसके लिए तो वह परमात्मा का ही प्रतीक है। मूर्ति में उसे अन्तर्यामी भगवान् की विद्यमानता की ही प्रतीति होती है। दक्षिण भारत के सभी शैव नयनार सन्तों ने शिवमूर्ति अर्थात् लिंग की पूजा के माध्यम से ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया था। भक्त के लिए प्रतिमा चिद्घन होती है। वह उससे प्रेरणा ग्रहण करता है। प्रतिमा उसका मार्ग-दर्शन करती है। वह उससे वार्तालाप करती है और विभिन्न प्रकार से उसकी सहायता करने के लिए मानव-शरीर धारण करती है। दक्षिण भारत के मदुरै मन्दिर में भगवान् शिव की मूर्ति ने एक लकड़हारे तथा एक वृद्ध स्त्री की सहायता की। तिरुपति के मन्दिर की मूर्ति ने अपने भक्त के सहायतार्थमानव-रूप धारण कर न्यायालय में साक्ष्य दिया। इस प्रकार के चमत्कार तथा रहस्य केवल भक्तों के लिए ही बोधगम्य होते हैं।
जब प्रतिमाएँ सजीव हो उठीं
किसी भक्त या सन्त के लिए जड़ पदार्थ जैसी कोई वस्तु नहीं है। यहाँ जो-कुछ भी है, वासुदेव या चैतन्य है-"वासुदेवः सर्वं इति।" वस्तुतः भक्त प्रतिमा में प्रभु के ही दर्शन करता है। एक राजा ने नरसी मेहता की परीक्षा ली। उसने उनसे कहा- "ओ नरसी, यदि तुम भगवान् कृष्ण के सच्चे भक्त हो और यदि तुम्हारे कथनानुसार प्रतिमा स्वयं भगवान् कृष्ण है, तो तुम इसे गतिशील कर दो।" नरसी मेहता की प्रार्थना के फल-स्वरूप प्रतिमा गतिशील हो गयी। शिव-मूर्ति के सम्मुख रहने वाले पावन वृषभ नन्दी ने तुलसीदास द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण किया। मूर्ति मीराबाई के साथ क्रीड़ारत रहती थी। वह उसके लिए सजीव तथा चेतन थी।
जब अप्पय दीक्षितार दक्षिण भारत स्थित तिरुपति मन्दिर गये, तब वैष्णवों ने उनको मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया; किन्तु दूसरे दिन प्रातःकाल उन वैष्णवों ने देखा कि मन्दिर की विष्णु-मूर्ति शिव-मूर्ति में परिणत हो गयी है। मन्दिर का महन्त यह देख कर स्तब्ध रह गया। उसने अप्पय दीक्षितार से क्षमा माँगते हुए उनसे विनय की कि वे मूर्ति को पुनः विष्णु की मूर्ति में परिणत कर दें।
दक्षिण भारत के दक्षिण कनारा जनपद-स्थित उडिपि में कनकदास नामक एक महान् कृष्ण-भक्त रहते थे। जातिगत अकुलीनता के कारण उनके लिए मन्दिर-प्रवेश वर्जित था। वे मन्दिर की परिक्रमा करने लगे। ऐसा करते समय उन्हें मन्दिर के पीछे एक छोटी खिड़की दिखायी पड़ी। इस खिड़की के सामने बैठ कर वे आत्म-विभोर हो कर भगवान् कृष्ण का स्तुति-गान करने लगे। भगवान् कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति और उनके संगीत के लयबद्ध माधुर्य से आकर्षित हो कर वहाँ बहुत लोग एकत्र हो गये। विग्रह में प्रतिष्ठित भगवान् कृष्ण भी अपनी स्थिति परिवर्तित कर कनकदास की ओर उन्मुख हो गये जिससे वे उनका दर्शन कर सकें। इस घटना ने पुजारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। तीर्थयात्रियों को आज भी वह खिड़की और वह स्थान दिखाया जाता है जहाँ बैठ कर कनकदास ने स्तुति-गान किया था।
मूर्ति भगवान् से अभिन्न है; क्योंकि यह मन्त्र चैतन्य-जो स्वयं देवता है-की अभिव्यक्ति का वाहन है। मूर्ति के सम्बन्ध में भक्त में वही अभिवृत्ति अपेक्षित है जो यदि भगवान् उसे प्रत्यक्ष दर्शन दे कर उससे सुस्पष्ट स्वरों में वार्तालाप करें, तो वह प्रदर्शित करेगा।
वेदान्त और मूर्ति-पूजा
तथाकथित वेदान्ती को मन्दिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के सम्मुख नतमस्तक होने में लज्जा का अनुभव होता है। वह समझता है कि उसके साष्टांग दण्डवत् करने से उसका अद्वैत वाष्पवत् विलुप्त हो जायेगा। अप्पर, सुन्दरार तथा सम्बन्धार आदि प्रख्यात तमिल सन्तों के जीवन-वृत्त का अध्ययन करने से आपको ज्ञात हो जायेगा कि अद्वैत के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष में उनकी कितनी गहरी पैठ थी। यद्यपि वे सर्वत्र भगवान् शिव का दर्शन करते थे तथापि वे सभी शिव-मन्दिरों में जा कर शिव-मूर्ति के सम्मुख नतमस्तक होते थे और भजन गाया करते थे। ये भजन आज भी उपलब्ध हैं। तिरसठ नायनार सन्तों ने केवल 'चर्या' तथा 'क्रिया' के अभ्यास से ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया था। वे मन्दिर के फर्श पर झाडू लगाते, पुष्प-चयन करते, भगवान् के लिए माला गूँथते और मन्दिर में दीप जलाते थे। वे निरक्षर थे; किन्तु उन्हें आत्मसाक्षात्कार हुआ। वे व्यावहारिक योगी थे और उनके हृदय विशुद्ध भक्ति से. ओत-प्रोत थे। वे कर्मयोग के मूर्त रूप थे। उन्होंने समन्वययोग का अभ्यास किया था। उनके लिए मन्दिर की मूर्ति मात्र प्रस्तर-खण्ड न हो कर चिद्यन थी।
मधुसूदन स्वामी को अद्वैत-साक्षात्कार, स्वात्मैक्य-दर्शन तथा अद्वैत-भाव का बोध हो चुका था; किन्तु वंशीधर भगवान् कृष्ण के सगुण रूप के प्रति उनकी अत्यधिक अनुरक्ति थी।
तुलसीदास को सर्वव्यापी सत्ता का साक्षात्कार हो चुका था। उनमें वैश्व-चेतना थी। सर्वव्यापी निराकार भगवान् से उनका वार्तालाप हुआ करता था; किन्तु धनुर्धर भगवान् राम के प्रति उनका तीव्र अनुराग मिट नहीं पाया था। अपनी वृन्दावन-यात्रा में जब उन्होंने मुरलीधर कृष्ण की मूर्ति देखी, तब उन्होंने कहा- "इस मूर्ति के सम्मुख मैं नतमस्तक नहीं होऊँगा।" तत्क्षण ही भगवान् कृष्ण की मूर्ति ने भगवान् राम की मूर्ति का रूप धारण कर लिया और तब उन्होंने उसके सम्मुख अपना शीश झुकाया। तुलसीदास की भाँति तुकाराम को भी यह वैश्व-अनुभव प्राप्त था। वे अपने अभंग में कहते हैं- "जिस प्रकार गन्ने में मधुर रस व्याप्त रहता है, उसी प्रकार मैं अपने भगवान् को सर्वभूतों में व्याप्त देखता हूँ।" किन्तु वे अपने कूल्हों पर हाथ रखे हुए पण्ढरपुर के विठ्ठल भगवान् का उल्लेख सगुण रूप में ही करते हैं। मीरा को भी सर्वव्यापी कृष्ण से अपने तादात्म्य का भान था; किन्तु वह 'मेरे गिरिधर नागर' की धुन की आवृत्ति अनवरत रूप से किया करती थी।
उपर्युक्त तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि मूर्ति-पूजा के माध्यम से ईश्वर-साक्षात्कार सम्भव है तथा ईश्वर के सगुण रूप की उपासना उसके साक्षात्कार के निमित्त की जाने वाली उसके सर्वगत निराकार पक्ष की उपासना में भी अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है। हम इस निष्कर्ष पर भी पहुँचते हैं कि प्रारम्भ में चित की एकाग्रता एवं ध्यान के लिए मूर्ति-पूजा अनिवार्य है और उपासना की इस विधि से भागवत-चेतना की सम्प्राप्ति में किसी भी प्रकार कोई अवरोध नहीं उपस्थित होता। जो लोग मूर्ति-पूजा के घोर विरोधी हैं, वे अज्ञान के निविड़ अन्धकार में भटक रहे होते हैं। पूजा और उपासना के यथार्थ ज्ञान से वंचित ये लोग मात्र विद्वत्ता-प्रदर्शन के लिए मूर्ति-पूजा के विरुद्ध अर्थहीन तथा अनावश्यक परिचर्चा और वाद-विवाद में संलग्न रहते हैं। यथार्थ साधन-सम्पत्ति के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता। अर्थहीन शब्दावली से बोझिल भाषा में सारहीन प्रवचन देना उनका स्वभाव तथा व्यवसाय बन गया है। अपने साथ-साथ उन्होंने अन्य अगणित लोगों के भी मन-मस्तिष्क को विकृत तथा अस्थिर करके उनका सर्वनाश कर दिया है। किसी-न-किसी रूप में समस्त संसार प्रतीकों और मूर्तियों की पूजा करता है। प्रारम्भ में मन को किसी स्थूल विषय या प्रतीक पर स्थिर करके उसे अनुशासित किया जाता है। जब यह स्थिर तथा सूक्ष्म हो जाता है, तब इसे 'अहं ब्रह्मास्मि' जैसी अमूर्त अवधारणाओं पर केन्द्रित किया जा सकता है। जैसे-जैसे साधक ध्यान के अभ्यास में प्रगति करता जाता है, वैसे-वैसे उसके लिए सगुण निर्गुण में परिणत हो जाता है और वह निराकार सत्ता से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। मूर्ति-पूजा वेदान्त की मान्यताओं के विरुद्ध नहीं है। इसके विपरीत यह उसकी सहायिका ही है।
जो लोग मूर्ति-पूजा के दर्शन तथा इसकी अर्थवत्ता से अभी तक अपरिचित थे, अब उन्हें इसका स्पष्ट बोध हो जायेगा और उनके ज्ञान-चक्षु खुल जायेंगे। शास्त्राध्ययन के विपरीत तथा योगियों, सन्तों के सम्पर्क से दूर रहने वाले अज्ञानी जन ही मूर्ति-पूजा के विरुद्ध अनावश्यक तर्क प्रस्तुत करते हैं।
कर्मकाण्डीय (वैधी) भक्ति से परा-भक्ति की ओर
उच्चतर भक्ति या परा-भक्ति तथा निम्नतर भक्ति या कर्मकाण्डीय भक्ति ये भक्ति के दो भेद हैं। कर्मकाण्डीय भक्ति को वैधी या गौणी-भक्ति कहते हैं। यह औपचारिक भक्ति है। वैधी-भक्ति भक्ति की निम्नतर विधा है जो बाह्य साधनों पर निर्भर है। इससे मन विशुद्धतर होता जाता है। इस भक्ति के द्वारा साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति क्रमशः प्रेम की वृद्धि होने लगती है। वह किसी प्रतीक या प्रतिमा की आराधना करता, घण्टी बजाता तथा पुष्प, चन्दन, धूप, दीपादि से प्रतिमा-पूजन कर ईश्वर को नैवेद्य अर्पित करता है।
मुख्या या परा-भक्ति भक्ति का एक विकसित रूप है। इसे उच्चतर भक्ति की संज्ञा दी गयी है। यह समस्त परम्पराओं का अतिक्रमण कर जाती है। भक्ति की इस विधा के प्रति आस्थावान् भक्त को किसी विधि-विधान की चिन्ता नहीं रहती। पूजा या उपासना के बाह्य प्रारूप के प्रति वह सर्वथा उदासीन रहता है। वह सर्वत्र और सर्वभूतों में अपने प्रभु के दर्शन करता है। उसका हृदय ईश्वर-प्रेम से ओत-प्रोत रहता है। उसके लिए अखिल विश्व वृन्दावन है। उसकी मनोदशा अनिर्वचनीय होती है और वह परम आनन्द को प्राप्त करता है। वह जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ-वहाँ प्रेम, विशुद्धता तथा आनन्द की किरणें विकीर्ण करता रहता है और जो कोई भी उसके सम्पर्क में आता है, उसके लिए वह प्रेरणाप्रद सिद्ध होता है।
प्रारम्भ में मूर्ति-पूजा करने वाले भक्त को अब सर्वत्र प्रभु के दर्शन होने लगते हैं और उसकी भक्ति परा-भक्ति का रूप ग्रहण कर लेती है। इसके फलस्वरूप वह वैधी-भक्ति की सीमाओं को पार करके रागात्मिका या प्रेमा-भक्ति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है। उसे सर्वभूतों में ईश्वर की प्रतीति होने लगती है तथा वह शुभ-अशुभ, शिव-अशिव आदि जैसे विचारों से मुक्त हो जाता है। दुष्ट, दस्यु, नाग, वृश्चिक, पिपीलिका, श्वान, वृक्ष, काष्ठ-खण्ड, शैल-राशि, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि में वह प्रभु का दर्शन करने लगता है। उसकी व्यापक दृष्टि तथा उसका दिव्य अनुभव वर्णनातीत है। ऐसे भक्तों की जय हो जो वस्तुतः भूसुर हैं और जो अन्य प्राणियों को सांसारिक पंक तथा मृत्यु-पाश से विमुक्त कर उन्हें उच्चतर स्थिति प्रदान करते हैं।
हिन्दू-धर्म जिज्ञासुओं को क्रमशः भौतिक प्रतीकों से मानसिक प्रतीकों की ओर, विविध मानसिक प्रतीकों से एकमेव सगुण ईश्वर की ओर तथा सगुण ईश्वर से परात्पर निर्गुण ब्रह्म की ओर ले जाता है।
हिन्दू-दर्शन की महिमा तथा हिन्दू-पूजा-पद्धति
हिन्दू-दर्शन तथा हिन्दू-पूजा-पद्धति कितनी उदात्त है! इसकी परिसमाप्ति प्रतिमा-पूजन में ही नहीं हो जाती। साधक मूर्ति-पूजा के माध्यम से भक्ति तथा समाधि के उच्च स्तरों तक पहुँच जाता है। मूर्ति-पूजा करते समय भी उसे सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान करना होता है। उसके लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने हृदय तथा सर्वभूतों में ईश्वर की विद्यमानता का भान होता रहे। एक लघु प्रतिमा का पूजन करते समय भी उसे पुरुष-सूक्त की आवृत्ति तथा उस सहस्रशीर्ष, सहस्रनेत्र और सहस्रवार विराट् पुरुष का चिन्तन करना होता है जो विश्व में व्याप्त होने के साथ-साथ इसका अतिक्रमण भी कर जाता है और जो नित्य-शुद्ध आत्मा या ईश्वर के रूप में सर्वभूतों में अवस्थित रहता है। जो व्यक्ति मूर्ति के सम्मुख धूप, अगरबत्ती तथा कर्पूर जलाता है, वही यह भी कहता है-"सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र तथा विद्युत् स्वयं दीप्तिमान् नहीं होते। ऐसी स्थिति में एक साधारण अग्नि-स्फुलिंग के लिए प्रकाशपूर्ण होना कैसे सम्भव है? वस्तुतः ये सब 'उसी' के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अखिल विश्व 'उसी' की दीमि से दीप्तिमान् है।" हिन्दू-शास्त्रों में वर्णित पूजा की विधियाँ तथा उसके रहस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी निर्भान्त तथा युक्तिसम्मत सिद्ध होते हैं। शास्त्राध्ययन तथा भक्तों एवं महात्माओं के सम्पर्क से वंचित अज्ञानी जन ही मूर्ति-पूजा की निन्दा करते हैं।
हिन्दू-धर्म से इतर प्रत्येक अन्य धर्म में कुछ निश्चित मत होते हैं जिनके अनुसरण के लिए लोगों को बाध्य किया जाता है। प्रत्येक ऐसे धर्म के पास सभी रोगों के उपचार के लिए एक ही औषधि होती है। समस्त स्थितियों के लिए तथा समस्त मनुष्यों के लिए एक ही प्रकार के भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है। समस्त अनुयायियों के लिए एक ही नाप का वस्त्र होता है। हिन्दू इस तथ्य से अवगत हैं कि मूर्ति, क्रास, द्वितीया का चन्द्रमा आदि प्रतीक मात्र हैं, जो प्रारम्भ में मन की स्थिरता तथा उसकी एकाग्रता के विकास के लिए उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें उन विभिन्न खूंटियों की भी संज्ञा प्रदान की गयी है जिन पर वे अपने आध्यात्मिक विचारों तथा अपनी आस्थाओं को लटका सकें। प्रतीक सबके लिए आवश्यक नहीं होता। हिन्दू-धर्म में इसे अनिवार्य नहीं माना गया है। उच्चतर स्थिति में योगियों एवं सन्तों के लिए यह अनावश्यक है। प्रतीक एक स्लेट की भाँति है जो प्रथम कक्षा के बाल-विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी होती है; किन्तु जिन लोगों के लिए यह अनुपयोगी है, उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि यह सबके लिए अनुपयोगी है। यदि वे इसे अनुपयोगी या व्यर्थ मानते हैं, तो इससे उनका अज्ञान ही परिलक्षित होता है।
निष्कर्ष
प्रारम्भ में मूर्ति-पूजा में कोई दोष नहीं होता। आपके लिए मूर्ति में ईश्वर तथा उसके गुणों का अध्यारोपण करना अनिवार्य है। आपकी चिन्तन-प्रक्रिया में इस तथ्य के लिए एक सुनिश्चित स्थान होना चाहिए कि मूर्ति में अन्तरात्मा निहित है। इसके पश्चात् साधक को शनैः -शनैः यह अनुभव होने लगता है कि उसके उपास्य प्रभु मूर्ति के साथ-साथ सर्वभूतों के हृदयों तथा विश्व के समस्त नाम-रूपों में भी अधिष्ठित हैं। उनकी विद्यमानता की प्रतीति उसे सर्वत्र होने लगती है।
मूर्ति-पूजा धर्म का इत्यलम् न हो कर इसका प्रारम्भ मात्र है। जो हिन्दू-शास्त्र नव-साधकों के लिए प्रारम्भ में मूर्ति-पूजा की अनुशंसा करते हैं, वही उच्चतर स्थिति के साधकों के लिए असीम या निरपेक्ष सत्ता के ध्यान की तथा 'तत्-त्वम्-असि' आदि महावाक्यों की अर्थवत्ता के चिन्तन की भी अनुशंसा करते हैं।
पूजा के विभिन्न सोपान हैं। प्रथम सोपान मूर्ति-पूजा तथा द्वितीय सोपान मन्त्रोच्चारण और प्रार्थना है। पुष्पार्चना की अपेक्षा मानसिक उपासना श्रेष्ठतर है। परम तत्त्व अथवा निर्गुण ब्रह्म का ध्यान सर्वतोत्कृष्ट है।
आत्म-साक्षात्कार या ब्रह्म-साक्षात्कार सर्वोच्च स्थिति है। ध्यान का स्थान द्वितीय है। योगी परमात्म-तत्त्व पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास करता है। उसके इस प्रयास में नैरन्तर्य होता है। मूर्ति-पूजा को तृतीय तथा यज्ञीय अनुष्ठानों एवं तीर्थाटन को चतुर्थ स्थान प्राप्त है। शास्त्र और गुरु दयामयी माता के समान हैं। वे साधकों के हाथ पकड़ कर पग-पग पर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और अपने इस अभियान में उस समय तक सक्रिय रहते हैं, जब तक साधक निर्विकल्प-समाधि को नहीं प्राप्त हो जाते। वे स्थूल-बुद्धि वाले नव-दीक्षित साधकों के लिए साधना की स्थूल विधियों का निर्धारण करते और विशुद्ध, सूक्ष्म तथा कुशाग्र बुद्धि से सम्पन्न उच्चतर स्थिति के साधकों को अमूर्त ध्यान की विधि का प्रशिक्षण देते हैं।
इनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक प्रगति के एक विशेष चरण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। मानवीय आत्मा अपनी शक्ति तथा अपने क्रमविकास की न्यूनाधिक मात्रा के अनुरूप असीम या निरपेक्ष सत्ता को ग्रहण करने या उसका साक्षात्कार करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करता है। वह उच्च से उच्चतर स्थिति को प्राप्त करता हुआ, अधिकाधिक शक्ति-संचय करता हुआ अन्ततः उस सर्वोच्च सत्ता में स्वयं को विलीन कर उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है।
उन हिन्दू-शास्त्रों तथा हिन्दू-ऋषियों की जय हो जो साधकों की उपासना को क्रमशः उच्चतर स्थितियों में ले जाते हुए अन्ततः उन साधकों को निर्गुण, सर्वव्यापी, निराकार, दिक्कालातीत (या उपनिषदों में वर्णित) असीम तथा निरुपाधिक ब्रह्म में संस्थित होने में सहायता प्रदान करते हैं!
ईश्वर की प्रिय सन्तानो ! अपनी अज्ञान-जनित अविश्वास की धारणा नष्ट करके इस क्षण अपने हृदय में उच्च, अडिग और जीवन्त आस्था को बद्धमूल कर लें। आप लोग मीरा, श्री रामकृष्ण परमहंस एवं दक्षिण भारत के अलवार तथा नयनार सन्तों का पुनः स्मरण करें। इन लोगों में आस्था थी और ये उच्चतम आध्यात्मिक सम्पदा के स्वामी थे। यदि आप लोग मूर्ति-पूजा के प्रति इसी प्रकार आस्थावान् हैं, तो आप लोग भी गहन शान्ति, सुख तथा समृद्धि का उपभोग करते हुए यहीं और इस क्षण परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं।
यद्यपि आप लोग नियमित रूप से बाह्य पूजा करते रह सकते हैं; परन्तु भगवान् की मानसिक पूजा (आन्तरिक पूजा) अनवरत और अबाध रूप से करते रहें। इससे उपासना पूर्ण हो जाती है। जीवन दैवी उपासना है। मेरी कामना है कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में विराट् की वैश्व उपासना के निहितार्थ से परिचित हो कर इसके अभ्यास द्वारा श्रेय तथा प्रेय को प्राप्त करें! आप सबको परमात्मा का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो!
अष्टम अध्याय
हिन्दू-योग
चार मार्ग
कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग तथा ज्ञानयोग-ईश्वर-साक्षात्कार के लिए, इन बारप्रमुख मांगों की व्यवस्था है। क्रियाशील प्रकृति के व्यक्तियों के लिए कर्मयोग, -मार्ग के प्रति आस्थावान् व्यक्तियों के लिए भक्तियोग, रहस्यवादी प्रकृति के तों के लिए राजयोग और बुद्धिवादी एवं दार्शनिक जिज्ञासुओं के लिए ज्ञानयोग अयुक्त है।
योग के अन्तर्गत मन्त्रयोग, लययोग या कुण्डलिनीयोग, लम्बिकायोग तथा हायोग की भी गणना होती है। योग का निहितार्थ वस्तुतः ईश्वर से तादात्म्याराथ तथा संयोगाभ्यास साधक को ईश्वर से सम्पर्क-स्थापन के लिए अभिप्रेरित करता है। इसकी प्रारम्भिक विधाओं में वैभिन्य होते हुए भी इनके लक्ष्य अभिन्न हैं।
कर्मयोग निष्काम सेवा का मार्ग है। निष्कामकर्मी को कर्मयोगी कहा जाता है। प्रकियोग भगवान् के प्रति एकान्तिक निष्ठा का मार्ग है। प्रेम तथा भक्ति के माध्यम से देवा-सायुज्य के अन्वेषी को भक्तियोगी कहा जाता है। राजयोग आत्मनिग्रह का मार्ग है। जो रहस्यवादी विधियों अर्थात् राजयोग द्वारा ईश्वर से तादात्म्य-स्थापन के लिए उपलशील रहता है, वह राजयोगी है। ज्ञानयोग ज्ञान-मार्ग है। जो दर्शन तथा जिज्ञासा के माध्यम से सर्वोच्च सत्ता से तदाकारिता की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है, उसे ज्ञानयोगी कहते हैं।
कर्मयोग
(कर्तव्य कर्तव्य के लिए)
कर्मयोग विहित क्रियाशीलता एवं निष्काम सेवा का मार्ग है। यह निष्काम कर्म द्वारा भगवत्प्राप्ति का मार्ग है। इसे कर्मफलों के प्रति अनासक्ति का योग कहते हैं।
कर्मयोग हमें कर्म के आसक्ति-रहित अनुष्ठान तथा अपनी अधिकाधिक शक्ति द्वारा सर्वोत्तम लक्ष्य की सम्प्राप्ति का कौशल प्रदान करता है। 'कर्तव्य कर्तव्य के लिए यह कर्मयोगी का आदर्श वाक्य है। कर्मयोग के अभ्यासी के लिए कर्म ही पु है। कर्मयोगी अपने प्रत्येक कर्म को हवन सामग्री का रूप प्रदान कर ईश्वर को कर देता है। वह कर्म-श्रृंखला में आबद्ध नहीं होता, क्योंकि वह अपने कमाँ के को ईश्वर को अर्पित कर देता है। "योगः कर्मस कौशलम्" अर्थात् योग कर्मक कौशल है।
सामान्यतः सुख-दुःख कर्म फल के अनुगत होते हैं। प्रत्येक कर्म सांसारिक के बन्धन को अधिकाधिक सम्पुष्ट करते हए अनेक जन्मों का कारण बनता है। य कर्मयोग के अभ्यास से कर्म के प्रभाव निर्लिप्त रहा जा सकता है। इस स्थिति में कर्म निर्बीज हो जाता है। जो कर्म कर्तापन के अहभाव से मुक्त, कर्मफलों के प्रति निरासक्त तथा सफलता-विफलता में सन्तुलित मैन हो कर समत्व-दृष्टि, सम्यक् मानसिक अभिवृत्ति, सम्यक् भाव तथा सम्क संकल्प द्वारा किया जाता है, वह बन्धन का कारण नहीं होता। इसके विपरीत वह हमारे हृदय को पावन करते हुए दिव्य प्रकाश के अवतरण या ज्ञानयोग के माध्यम से हमने लिए मुक्ति-प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है।
कर्मयोग के अभ्यास के लिए कठोर नैतिक अनुशासन तथा इन्द्रिय-निग्रह अनिवार्य है।
वस्तुतः ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त सहिष्णुता, सामंजस्य, सहानुभूति, दया, समदृष्टि, मानसिक सन्तुलन, विश्व-प्रेम, धैर्य, दृढ़ता, विनम्रता, उदारता, उदात्तता, आत्मनिग्रह, क्रोधानुशासन, अहिंसा, सत्य, खान-पान तथा निद्रा में मिताचार, सादा जीवन तथा तितिक्षा जैसे सद्गुणों का अर्जन भी अत्यन्त आवश्यक है।
प्रत्येक मनुष्य को अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार स्व-धर्म का पालन करना चाहिए। पर-धर्म के प्रति आकर्षित हो कर स्व-धर्म का परित्याग श्रेयस्कर नहीं होता।
कुछ लोगों के अनुसार कर्मयोग एक निम्न कोटि का योग है। वे सोचते हैं कि पानी लाना, बरतन साफ करना, निर्धनों को भोजन देना और फर्श पर झाडू लगाना भृत्योचित कर्म हैं; किन्तु यह एक दु खद भूल है। वस्तुतः ये लोग कर्मयोग की प्रविधि तथा महिमा से नितान्त अपरिचित होते हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान् कृष्ण को अर्जुन के सारथि का कार्य-भार ग्रहण करने के अतिरिक्त गोपालन-कर्म भी करना पड़ा था।
भक्तियोग
(प्रेम प्रेम के लिए)
भगवान् के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्तियोग भक्ति का मार्ग है। इसके प्रति अधिकांश लोग आकर्षित होते हैं। 'प्रेम प्रेम के लिए'-भक्तियोगी का मिर्गदर्शक सूत्र है। परमात्मा प्रेम का मूर्त रूप है। उसके प्रति प्रेम ही उसकी प्राप्ति में सहायक होगा। भावावेशपूर्ण दाम्पत्य प्रेम की भाँति तीव्र एवं उत्कट प्रेम द्वारा ही ईश्वर-साक्षात्कार सम्भव है। भगवत्प्रेम के विकास की गति आनुक्रमिक ही होनी चाहिए।
जिसका ईश्वर के प्रति प्रेम-भाव है, वह दुःखी और अभावग्रस्त नहीं होता। वह किसी प्राणी या वस्तु से घृणा नहीं करता। विषय-वासना से उसे आनन्द नहीं प्राप्त होता। वह अपने उत्कट प्रेमालिंगन में सबको आबद्ध कर लेता है।
काम तथा तृष्णा भक्ति के प्रतिबन्धक हैं। जब तक आपके मन में कामना का लेशमात्र भी अवशेष है, तब तक आपके ईश्वर-प्रेम में तीव्रता नहीं आ सकती।
आत्मनिवेदन भगवान् के प्रति पूर्ण, अकृत्रिम तथा निरपेक्ष आत्मसमर्पण है। यह नवधा-भक्ति का उच्चतम प्रारूप है। आत्मनिवेदन प्रपत्ति अथवा शरणागति है। प्रपत्ति के द्वारा भक्त भगवान् से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उसे ईश्वरीय अनुग्रह या प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है।
ईश्वर के प्रति प्रेम तथा सखा-भाव-जनित आनन्दातिरेक का सम्यक् वर्णन काब्दों द्वारा असम्भव है। यह स्थित्ति उस मूक व्यक्ति की-सी स्थिति है जो स्वादिष्ट नोजन कर लेने के बाद स्वयं को भोजन के स्वाद-वर्णन में सर्वथा असमर्थ पाता है। इसकी अनावृति कुछ विशिष्ट जनों के लिए ही सम्भव है। जिसको एक बार यह समानुभूति हो चुकी है, एकमात्र वही उसके दर्शन, उसके श्रवण तथा उसके वर्णन में समर्थ हो सकेगा; क्योंकि वह अनवरत रूप से उसी का चिन्तन करता रहता है।
आध्यात्मिक विज्ञानों में भक्ति एक प्रमुख विज्ञान है। परमात्मा के प्रति जिसका नम है, वह वस्तुतः एक समृद्धि-सम्पन्न व्यक्ति है। भगवत्प्रेम के अभाव के अतिरिक्त अन्य कोई भी दुःख नहीं है। भगवान् के प्रति भक्त का प्रेम ही एकमात्र सम्यक् मार्ग है। नरमात्मा का नाम, उसके गुण तथा उसकी लीलाएँ सतत स्मरणीय हैं। उसके चरण-कमल ध्यान के मुख्य विषय हैं। भक्त भगवत्प्रेम का अमृत-पान करता है।
भक्तों में जातिगत, विश्वासगत, परिवारगत, वर्णगत या प्रजातिगत पार्थक्य नहीं होता। इन बातों की ओर परमात्मा का ध्यान नहीं जाता। वह भक्तों के हृदय की विशुद्धता को ही देखता है। कोई भी व्यक्ति भगवद्भक्त हो सकता है। अस्पृश्य नन्दा, चर्मकार रैदास, आखेटधर्मी कण्णप्प, नाई सेना, मुसलमान बुनकर कबीर और भीलनी शबरी ये सभी भगवान के भक्त तथा महान् सन्त थे। आखेटधर्मी कण्णप्प एक निरक्षर तथा बर्बर व्यक्ति था। उसने मुँह में जल भर कर शिव-लिंग पर चढ़ा दिया था नैवेद्य अर्पित कर दिया था; किन्तु श्रेष्ठतम भक्तों में की जाती है। दक्षिण भारत के वैष्णव अलवार तथा शैव नयनार समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों के सदस्य थे।
राजयोग
(चित्त-वृत्ति-निरोध)
राजयोग आत्मनिग्रह तथा मन के नियन्त्रण के माध्यम से परमात्मा से सायुज्य-स्थापन की विधा है। यह हमें इन्द्रियों के नियम तथा चित्त से निःसृत होने बाली विचार-तरंगों अर्थात् चित्तवृत्तियों के निरोध, एकाग्रता के विकास तथा ईश्वर-सान्निध्य की कला में प्रशिक्षित करता है। हठयोग में शरीर तथा राजयोग में मन को प्रशिक्षित किया जाता है।
अष्टांगयोग
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि राजयोग के अष्टांग हैं।
यम तथा नियम की गणना उस नैतिक अनुशासन के अन्तर्गत की जाती है जिससे चित्त-शुद्धि होती है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह के सम्मिलित रूप को यम के नाम से जाना जाता है। ये सभी गुण अहिंसा में बद्धमूल हैं।
कुछ विशिष्ट व्रतों या विधियों के अनुपालन को नियम कहा जाता है। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान नियम के अन्तर्गत आते हैं। यम तथा नियम में स्थित साधक योगाभ्यास में त्वरित गति से प्रगति करता है।
आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार को योग के अतिरिक्त साधन के रूप में व्यवहत किया जाता है। आसन स्थिर मुद्रा तथा प्राणायाम श्वास-प्रश्वास का नियमन है। इससे शान्ति, मन की स्थिरता तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। विषयों से इदियों की विमुखता प्रत्याहार है। आपके लिए प्रत्याहार का अभ्यास आवश्यक है; हयाँकि एकमात्र इसी के द्वारा आपको अन्तर्दृष्टि तथा अन्तर्मुखता की सम्प्राप्ति होगी है।
किसी बाह्य विषय, अन्तश्चक्र अथवा किसी इष्ट या अधिष्ठातृ देवता पर मन की स्थिरता को धारणा कहते हैं। इसके पश्चात् आता है ध्यान। यह किसी एक विषय तर केन्द्रित विचारों का सतत प्रवाह है। ध्यान द्वारा साधक समाधि की दिशा में अग्रसर होता है। समाधि में ध्याता तथा ध्येय एक हो जाते हैं। इस स्थिति में चित्तवृत्तियाँ वितान्त क्षीण, मन सर्वथा निष्क्रिय एवं संस्कार-समुदाय तथा वासनाएँ पूर्णतः विनष्ट हो जाती हैं और योगी जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो कर कैवल्य प्राप्त कर लेता है।
चित्त की एकाग्रता-सफलता की कुंजी
सर्चलाइट में कितनी शक्ति होती है! एक विशिष्ट विधि से निर्मित काँच (लेन्स) का केन्द्रीभूत सूर्य की किरणें रूई को जला सकती हैं। इसी प्रकार आप भी चित्त की बबाल वृत्तियों को एक विषय पर केन्द्रित कर चमत्कारों की सृष्टि और इसके प्रकाश द्वारा प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में बैठ कर अपनी सारी शक्ति को एक बिन्दु पर एकत्र कर अपने शोध तथा अनुसन्धान के विषय पर केन्द्रित कर देता है। इसके फलस्वरूप उसे तत्त्वादि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह प्रकृति के समस्त प्रच्छन्न रहस्यों को हस्तामलकवत् अनावृत कर देता है। ज्योतिषी भी यही करता है। वह अपने दूरदर्शक-यन्त्र के माध्यम से ग्रह-नक्षत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर नक्षत्र-विज्ञान से परिचित हो जाता है। रेडियो, बेतार का तार, तार, दूरदर्शन, ग्रामोफोन, दूरभाष, भाप के इंजन आदि सारे आविष्कार गहन एकाग्रता द्वारा ही सम्भव हो सके हैं।
चित्त की एकाग्रता के अभाव में आप आध्यात्मिक साधना या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। मन बन्दर की भाँति चंचल है। यदि रसोइये का चित्त एकाग्र है, तो वह कुशलतापूर्वक भोजन तैयार कर सकता है; किन्तु यदि उसमें एकाग्रता नहीं है, तो वह भोजन नितान्त अरुचिकर और स्वाद-गन्ध-हीन हो जायेगा। शल्य-चिकित्सा-कक्ष में शल्य-चिकित्सक को और जलपोत में पोतचालक को पूर्ण आय से एकाग्र-चित्त होने की आवश्यकता होती है। दर्जी, अध्यापक, विधिवेत्ता तथा विद्यार्थी-इन सभी में चित्त की एकाग्रता अनिवार्य है। एकाग्र-चित्त हो कर ही वे माने व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। महान् कार्यों के निष्पादन में सफल सभी महान् हा मेधावी व्यक्तियों में चित्त की एकाग्रता पूर्ण रूप से विद्यमान थी।
सांसारिक विषयों में रत मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ बहिर्मुखी होती हैं। उसका मन बन्दर की भाँति चंचल रहता है। वह सर्वदा अशान्त रहता है। धन, खी, सन्तान, सम्पत्ति, गृहादि मात्र उसके चिन्तन के विषय होते हैं। उसका मन धनोपार्जन एवं अपनी इच्छित वस्तुओं की सम्प्राप्ति में सदैव व्यस्त रहता है। चित्त की एकाग्रता का उसमें नितान्त अभाव होता है। अन्तर्दृष्टि तथा आत्म-विश्लेषण उसके लिए दुर्लभ हैं। उसका मन बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का आश्रय स्थान बना रहता है।
योगी अपने चित्त को चक्रों, मन, सूर्य, नक्षत्रों तथा तत्त्वादि पर स्थिर कर अधिमानवीय ज्ञान प्राप्त करता है। वह तत्त्वों पर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। चित्त की एकाग्रता ही ज्ञान के कोषागार के ताले की एकमात्र कुंजी है।
चित्त की एकाग्रता की प्राप्ति एक सप्ताह या मास में सम्भव नहीं है। इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता तो होती ही है। इसके अभ्यास में नियमितता का सर्वोपरि महत्त्व है। ब्रह्मचर्य, शान्त तथा मनोनुकूल स्थान, सन्तों की संगति एवं सात्विक आहार चित्त की एकाग्रता के सहायक उपकरण हैं।
चित्त की एकाग्रता तथा ध्यान द्वारा साधक समाधि की दिशा में अग्रसर होता है। वितर्क, विचार, आनन्द तथा अस्मिता समाधि के विकास-क्रम की विभिन्न अवस्थाएँ हैं। इस प्रकार इन अवस्थाओं को आक्रान्त करने के पश्चात् कैवल्य का प्रसाद प्राप्त होता है।
सिद्धियाँ अवरोधक भी हो सकती हैं
योगाभ्यास में योगी की प्रगति के फल-स्वरूप उसे सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। दूरदर्शन तथा दूरश्रवण आदि जैसी सिद्धियाँ योगी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। उसे चाहिए कि वह इनकी निर्मम उपेक्षा करते हुए अपने लक्ष्य, असम्प्रज्ञात या निर्विकल्प-समाधि की दिशा में अव्यवहित गति से अग्रसर होता रहे। यथार्थ आध्यात्मिकता से इन सिद्धियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। ये तो चित्त की एकाग्रता के गौण फल मात्र हैं। इन सिद्धियों का अनुगमन करने वाला सांसारिकता या गृहस्थाश्रम के अविहित कर्मों में लिप्त व्यक्ति है। यदि वह सतर्क नहीं है, तो उसका पतन निश्चित है।
ज्ञानयोग
(आध्यात्मिक अन्तर्दर्शन का मार्ग)
ज्ञानयोग ज्ञान का मार्ग तथा ब्रह्मज्ञान मोक्ष-प्राप्ति का साधन है। जीवात्मा के परमात्मा अर्थात् ब्रह्म से तादात्म्य की प्रतीति या अनुभव से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अविद्या बन्धन तथा दुःख का कारण है। अविद्या के कारण क्षुद्र जीव मूर्खतावश स्वयं को बारा से पृथक समझ लेता है। अविद्या की आवरण-शक्ति के सरला का स्वतं अपने यथार्थ दिव्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। ब्रह्मज्ञान इस आवरण को नह को उसे शत्-चित्-आनन्द-स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देता है।
आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि तथा बौद्धिक ज्ञान
ज्ञानयोगी इस सत्य से परिचित हो जाता है कि ब्रह्म उसके जीवन का जीवन तापी उसकी आत्मा की आत्मा है। उसे इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा उसका आत्मस्वरूप है। आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि या अन्तःप्रज्ञा से उसे शाश्वत सत्ता से इतनी अभिन्नता की अपरोक्षानुभूति हो जाती है। वह यह भी समझ रहा होता है कि अभावलोकन तथा सिद्धान्तों के प्रति आग्रहशीलता मात्र से यह सम्प्राप्ति असम्भव है। धावं अब उसके लिए अर्थहीन वार्तालाप का विषय न हो कर अनुभूति का विषय हो जाता है। वह सतत तथा गहन ध्यान अर्थात् निदिध्यासन के माध्यम से हृदय की गहनतम गुहा में प्रविष्ट हो कर उस आश्चर्यजनक आत्म-मुक्ता को, उस आश्चर्यजनकी निधि को प्राप्त कर लेता है जिसके समक्ष संसार की सारी सम्पत्ति नगण्य है।
ज्ञान केवल बौद्धिकता-प्रसूत ज्ञान नहीं है। यह श्रवण तथा स्वीकृति मात्र नहीं है। यह केवल बौद्धिक सहमति न हो कर चरम सत्ता से जीव की एकत्व-भावना की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसे परा-विद्या कहते हैं। मात्र बौद्धिक ज्ञान आपको ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकता।
ज्ञानयोग का साधक सर्वप्रथम साधन-चतुष्टय अर्थात् विवेक, वैराग्य, -सम्पत् तथा मुमुक्षुत्व से सम्पन्न होता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधान को षट्-सम्पत् कहते हैं। साधन-चतुष्टय से सम्पन्न साधक गुरु के चरणकमलों में बैठ कर उससे श्रुतियों का श्रवण-लाभ करता है। गुरु मात्र श्रोत्रिय न हो कर ब्रह्मनिष्ठ भी होता है। इसके पश्चात् साधक मनन का अभ्यास करता है जिसके फलस्वरूप उसके सभी संशयों की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। तदनन्तर वह ब्रह्म के गहन ध्यान अर्थात् निदिध्यासन द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार कर लेता है जिसके फलस्वरूप वह जीवन्मुक्त हो जाता है। शरीरस्थ होते हुए भी उसे मुक्ति का प्रसाद प्राप्त हो जाता है।
शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसी, सत्त्वापत्ति, असंसक्ति पदार्थाभावना एवं तुर्यगा अथवा तुरीय ज्ञान की सप्त-भूमिकाएँ हैं।
दो पक्षियों का दृष्टान्त
एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक वृक्ष की सर्वोपरि शाखा पर है और दूसरा नीचे की शाखा पर। सर्वोपरि शाखा पर बैठा पक्षी सर्वदा शान्त, मौन तथा अपनी महिमा में अधिष्ठित रहता है। वह सर्वदा आनन्द-स्वरूप रहता है। किन्तु निम्नतर शाखा पर बैठा पक्षी क्रमशः मधुर तथा तिक्त फलों का रसास्वादन करता रहता है और कभी-कभी हर्षातिरेक में नृत्य भी करने लगता है। वह क्षण-क्षण में कभी सुखी और कभी दुःखी होता रहता है। कभी-कभी वह अत्यन्त तिक्त फल का आस्वादन कर उद्विग्न हो उठता है। वह ऊपर बैठे स्वर्णिम पंख वाले अद्भुत पक्षी का अवलोकन करता है जो सर्वदा अपने आनन्द-स्वरूप में स्थित रहता है। वह भी इस स्वर्णिम पंख वाले पक्षी का स्वरूप ग्रहण करना चाहता है; किन्तु शीघ्र ही उसकी यह इच्छा विस्मृत हो जाती है और वह पुनः मधुर-तिक्त फलों के रसास्वादन में लिप्त हो जाता है। वह पुनः एक दूसरा फल खाता है जो अत्यधिक तिक्त होता है। इसके फल-स्वरूप वह अत्यन्त दुःखी हो जाता है और एक बार पुनः वह ऊपर बैठे पक्षी के समतुल्य हो जाना चाहता है। क्रमशः वह फल-भक्षण का परित्याग कर देता है और ऊपर बैठे पक्षी की भाँति शान्त तथा आनन्द-स्वरूप हो जाता है। ऊपर बैठा पक्षी ईश्वर या ब्रह्म है, जब कि नीचे बैठा पक्षी जीव या जीवात्मा है जो अपने कर्मानुसार सुख-दुःख का फल भोगता है। जीवन-संघर्ष में आघात सहन करता हुआ वह आरोहण तथा अवरोहण की स्थिति को प्राप्त होता रहता है। वह ऊपर उठता है; किन्तु इन्द्रियों से सम्मोहित हो कर पुनः नीचे गिर जाता है। वह अनुक्रमिक रूप से विवेक तथा वैराग्य की साधन-सम्पदा अर्जित कर ईश्वरोन्मुख हो जाता है और ध्यान के अभ्यास द्वारा आत्मसाक्षात्कार का प्रसाद प्राप्त कर ब्रह्म के शाश्वत आनन्द का अनुभव करने लगता है।
समन्वययोग
कुछ लोगों के विचारानुसार कर्मयोग का अभ्यास ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। कुछ अन्य लोगों की यह मान्यता है कि ईश्वर-भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है और कुछ लोगों के विश्वासानुसार ज्ञान-मार्ग ही निरतिशय आनन्द की सम्प्राप्ति का एकमेव पथ है। किन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तीनों मार्गों को पूर्णता एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए समान रूप से प्रभावप्रद समझते हैं।
मनुष्य संकल्प, भावना तथा विचार का एक विचित्र मिश्रण है। वह अपनी आकांक्षित वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसमें संवेग है जिससे उसमें भावनाओं का उद्रेक होता है। उसमें बुद्धि तथा विवेक हैं जिससे वह विचार तथा तर्क-वितर्क करता है। कुछ लोगों में संवेगात्मक तत्त्वों का प्राबल्य रहता है, जब कि कुछ लोग मुख्यतः विवेक-बुद्धि द्वारा अनुशासित होते हैं। जिस प्रकार संकल्प, भावना तथा विचार परस्पर अपृथक् है, उसी प्रकार कर्म, भक्ति तथा ज्ञान भी एक-दूसरे से अपृथक् हैं।
समन्वययोग साधना की सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रभावप्रद विधि है। मल, विक्षेप तथा आवरण-ये मन के विकार-त्रय हैं। मल का निराकरण कर्मयोग के अभ्यास से, विक्षेप की निवृत्ति उपासना से और आवरण का उच्छेदन ज्ञान-मार्ग से करना चाहिए। अात्मसाक्षात्कार का एकमात्र मार्ग यही है। दर्पण पर से धूल आदि हटा कर, उसे एक स्थान पर स्थिर कर तथा उसके बाह्य आवरण-पट को हटा कर ही आप उसमें अपक मुँह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सरोवर के तल में स्पष्ट प्रतिबिम्ब-दर्शन के लिए उसके पंक, वायु-प्रताड़ित जल के उद्वेलन तथा उसकी काई को नष्ट करना नितान्त आवश्यक है। यही बात आत्मसाक्षात्कार के सम्बन्ध में भी है।
समन्वययोग से ही सामंजस्यपूर्ण तथा समग्र विकास सम्भव हो सकेगा और एकमात्र उसी की साधना से शरीर, मस्तिष्क तथा हृदय सम्पुष्ट हो सकेंगे। मनुष्य के लिए पूर्णत्व-प्राप्ति का यही साधन है। प्रत्येक दिशा में सामंजस्यपूर्ण सन्तुलन ही धर्म का आदर्श है। इसकी सम्प्राप्ति समन्वययोग के अभ्यास से ही सम्भव होती है।
सभी जीवों में वैश्विक आत्मा का दर्शन ज्ञान है, इस वैश्विक आत्मा के प्रति प्रेम भक्ति है तथा इसकी सेवा कर्म है। ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् ज्ञानयोगी भक्ति तथा निष्काम कर्म से सम्पन्न हो जाता है। कर्मयोग उसकी आध्यात्मिक प्रकृति की एक सहज अभिव्यक्ति है; क्योंकि वह सर्वभूतों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। जब भक्त भक्तियोग में निष्णात होता है, तब वह ज्ञान तथा कर्म से भी सम्पन्न हो जाता है। उसके लिए भी कर्मयोग उसकी दिव्य प्रकृति की सहज अभिव्यक्ति हो जाता है; क्योंकि उसे ईश्वर के दर्शन सर्वत्र होते हैं। कर्मयोगी के लिए ज्ञान तथा भक्ति की सम्प्राप्ति तभी सम्भव होती है, जब उसके कर्म पूर्णतः निष्काम हो जाते हैं। ये तीनों मार्ग वस्तुतः एक ही हैं। इन तीनों में से प्रत्येक अपने शेष अविच्छेद संघटक तत्त्वों पर प्रधानता प्राप्त कर लेता है। योग से हमें उस विधि की प्राप्ति होती है जिससे हम आत्मदर्शन, आत्मप्रेम तथा आत्मसेवा में समर्थ हो पाते हैं।
नवम अध्याय
हिन्दू-धर्मविज्ञान
हिन्दू-धर्मविज्ञान-विषयक वर्गीकरण
हिन्दू-धर्म : विभिन्न मतों का मैत्री-संघ तथा विभिन्न दर्शनों का महासंघ
हिन्दू-धर्मविज्ञान मुख्यतः देवत्व के छह रूपों-गणेश, देवी (दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती), शिव, विष्णु, सूर्य तथा स्कन्द-की आराधना का अध्ययन तथा मत (doctrine) है। दिव्य आराधना के इन पक्षों को षण्मत कहा जाता है।
हिन्दू-धर्म सार्वभौम, उदार, सहिष्णु तथा लचीला है। यह इसका अद्भुत स्वरूप है। एक विदेशी हिन्दू-धर्म के नानाविध सम्प्रदायों एवं मतों के नाम सुन कर आश्चर्यचकित रह जाता है; किन्तु यह विविधता हिन्दू-धर्म का दोष न हो कर इसका गुण या इसकी शोभा ही है। लोगों में मनोगत एवं स्वभावगत वैभिन्य होता है; अतः विभिन्न आस्थाओं का होना भी आवश्यक है। यह हिन्दू-धर्म का मूलभूत सिद्धान्त है जो स्वाभाविक भी है। इस धर्म में उच्चतर से ले कर निम्नतम आत्माओं तक की अभिवृद्धि और उनके विकास के लिए पर्याप्त स्थान है।
हिन्दू-धर्म अत्यन्त लचीला है। यह अनेक सम्प्रदायों एवं उपासना-पद्धतियों को स्वयं में सँजोये हुए है; किन्तु अनेक महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर इसमें परस्पर भेद भी हो जाता है। हिन्दू-धर्म में वेदान्त, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि अनेक मत सन्निहित हैं। यह अनेक मतों एवं उपासना-पद्धतियों का पुंज है। यह किसी निश्चित मत के प्रति आग्रहशील कोई धर्म-विशेष न हो कर धर्मों का एक महासंघ है। इसके द्वार सभी के लिए खुले हैं। इसमें योग्यता एवं विकास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन की व्यवस्था है। उदार धर्म का सौन्दर्य इसी में सन्निहित रहता है और यही है हिन्दू-धर्म की महिमा। अतः यहाँ विभिन्न मत-मतान्तरों में किसी प्रकार के विरोध के दर्शन नहीं होते। ऋग्वेद की उद्घोषणा है : "एकं सद्विप्राः बहुधा चदन्ति" अर्थात् सन्त जन एक ही सत्य को पृथक् पृथक् नामों से पुकारते हैं। उपनिषदों की मान्यता है कि जिस प्रकार पृथक् पृथक् रंगों वाली गायों के दूध का रंग एक अर्थात श्वेत ही होता है, उसी प्रकार सभी धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गों का गन्तव्य भी एक ही होता है। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं: मनुष्य किसी भी मार्ग से मुझ तक क्यों न पहुँचे, मैं उसको शरण देता हूँ, क्योंकि वे सारे मार्ग मेरे ही में समाहित हो कर सारी
इस प्रश्न का उत्तर कठिन है कि हिन्दू-धर्म है क्या? यह आस्थाओं का क्षेत्री-संघ तथा दर्शनों का महासंघ है। यह विश्व के विभिन्न मतावलम्बी विचारको हीथा दार्शनिकों के चिन्तन के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है। सभी दर्शन आवश्यक है। एक व्यक्ति के लिए जो दर्शन आकर्षक और सरल-सहज हो सकता है, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनाकर्षक और दुर्बोध हो सकता है। अतः विभिन्न दृष्टिकोण आवश्यक हैं। हिन्दू-धर्म के सभी दर्शन विभिन्न दृष्टिकोण ही हैं। ये जिज्ञासुओं को उच्च से उच्चतर स्तरों की ओर अग्रसरण की प्रेरणा देते हुए उन्हें आध्यात्मिक महिमा के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ करवा देते हैं।
सनातनधर्मी, आर्यसमाजी, देवसमाजी, जैन, बौद्ध, सिक्ख और ब्रह्मासमाजी-ये सभी हिन्दू ही हैं; क्योंकि इनका प्रादुर्भाव हिन्दू-धर्म से ही हुआ है और ये हिन्दू-धर्म के एकाधिक पक्षों को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं।
हिन्दू वैष्णव, शैव तथा शाक्त-इन तीन महान् एवं महत्त्वपूर्ण सम्प्रदायों में विभाजित हैं जो क्रमशः विष्णु, शिव तथा भगवती मातृ देवी के उपासक हैं। इनके अतिरिक्त सौर्य, गाणपत्य तथा कौमार भी हैं जो क्रमशः भगवान् सूर्य, गणेश तथा स्कन्द को ईश्वर मान कर उनकी उपासना करते हैं।
वैष्णव
श्री-सम्प्रदायी
वैष्णव सामान्यतः चार प्रमुख सम्प्रदायों में विभक्त हैं। इनमें रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित श्री-सम्प्रदाय प्राचीनतम है। रामानुजाचार्य के अनुयायी विष्णु भगवान्, लक्ष्मी तथा इनके अवतारों की आराधना करते हैं। इनको रामानुजी, श्रीसम्प्रदायी या श्री वैष्णव कहा जाता है। ये लोग 'ॐ नमो नारायणाय' अष्टाक्षर-मन्त्र का जप करते और मस्तक पर दो रेखाओं के मध्य एक लाल रंग की रेखा का तिलक लगाते हैं।
रामानुजाचार्य के वेदान्त देशिक नामक एक अनुयायी ने वैष्णव-मत में कुछ सुधार किये जिनके फलस्वरूप रामानुजी दो दलों में विभक्त हो गये। इनमें एक को बडगलाई (उदीच्य-मत) और दूसरे को तेंगलाई (दाक्षिणात्य-मत) कहा जाता है। तेंगलाई प्रपत्ति या आत्मसमर्पण को ही मोक्ष का एकमात्र साधन समझते हैं। वडगलाई इसे मात्र अनेक साधनों में से एक साधन मानते हैं। वडगलाई मत के अनुसार भक्त एक बानर-शिशु की भाँति होता है जो अपनी माँ के साथ स्वयं चिपका रहता है (मर्कट-न्याय); किन्तु दाक्षिणात्य-मत के अनुसार भक्त एक मार्जार-शावक की भाँति होता है जो माँ द्वारा बिना प्रयास के ही इतस्ततः ले जाया जाता है (मार्जार-न्याय)। उदीच्य-मत को संस्कृत भाषा में लिखित वेद मान्य हैं; किन्तु दाक्षिणात्यों ने तमिल भाषा में 'नालायिर प्रबन्धम्' (चतुःसहस्रपदी) नामक अपने निजी वेदों की रचना कर ली है जिसे वे संस्कृत में लिखित वेदों से प्राचीन समझते हैं। वस्तुतः उनका 'नालायिर प्रबन्धम्' वेदों के औपनिषदिक भाग पर ही आधारित है। वे अपनी सभी उपासनाओं में इसके पदों का गायन करते हैं।
वडगलाई मतानुसार लक्ष्मी को विष्णु की सहधर्मिणी मानते हैं जो स्वयं अनन्त तथा अजन्मा हैं। वे यह भी मानते हैं कि विष्णु की आराधना की भाँति उनकी आराधना भी मोक्ष का उपाय अर्थात् साधन है। तेंगलाई मतानुयायी लक्ष्मी को जन्मशीला किन्तु दिव्यरूपिणी मानते हैं। उनके मतानुसार ये स्वयं मुक्तिप्रदायिका न हो कर मुक्ति-प्राप्ति के लिए मध्यस्थ मात्र हैं।
दोनों मतों में मस्तकीय तिलक-चिह्नों में भी भेद है। वडगलाई मतानुयायी अपने मस्तक पर अँगरेजी U अक्षर के आकार का श्वेत तिलक लगाते हैं, जो गंगा जी के उद्गम स्थान भगवान् विष्णु के दक्षिण चरण-तल का प्रतीक है। वे इसके मध्य में लाल रंग का एक चिह्न चित्रित करते हैं जो लक्ष्मी का प्रतीक है। तेंगलाई मतानुयायी अँगरेजी के Y अक्षर-जैसा चिह्न अंकित करते हैं जो भगवान् विष्णु के चरण-द्वय का प्रतिनिधित्व करता है। वे नासिका के मध्य भाग तक एक श्वेत रेखा का अंकन करते हैं।
दोनों मतों के अनुयायी अपने वक्ष, कन्धों तथा अपनी बाँहों पर भगवान् विष्णु के प्रतीक चिह्न शंख तथा चक्र का चित्रांकन करवा लेते हैं।
तेंगलाइयों में विधवा का केश-मुण्डन वर्जित है। रामानुजी ब्राह्मणों के नाम के आगे सामान्यतः उपजाति-बोधक अय्यंगार, आचार्य, चालू तथा आचालू शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं।
रामानन्दी
रामानन्द के अनुयायियों को रामानन्दी कहते हैं। उत्तरी भारत के लोग इनसे भली विधि परिचित हैं। ये रामानुज-सम्प्रदाय की एक शाखा है। ये भगवान् राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान की उपासना करते हैं। रामानन्द रामानुज के शिष्य थे। लगभग चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक ये वाराणसी में प्रख्यात हो चुके थे। भारत में गंगा की घाटी में इनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। उनकी प्रिया कृते भक्ति-माल है। इनके सम्प्रदायगत चिह्न रामानुजियों की भाँति ही हैं। रामानन्दी- सम्प्रदाय के गृहत्यागी सन्तों को वैरागी कहा जाता है।
वल्लभाचारी अथवा कृष्ण-सम्प्रदायी
मुम्बई, गुजरात तथा मध्य भारत में वल्लभाचारी-सम्प्रदाय का अत्यधिक महत्व है। इसके प्रवर्तक का जन्म १४७९ में चम्पारण्य में हुआ था। उन्हें भगवान् कृष्ण का अवतार माना जाता है। वल्लभाचारी कृष्ण की आराधना बाल-गोपाल के रूप में करते हैं। वे उनके द्वादशवर्षीय बालरूप की प्रतीक प्रतिमा की आराधना करते हैं। गोसाईं या धर्मगुरु गृहस्थ होते हैं। ईश्वर-पूजन के लिए मन्दिरों में दैनिक अष्टविध अनुष्ठान अर्थात् मंगल, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, सन्ध्या तथा शयन का विधान है। ये सब ईश्वरोपासना के विभिन्न रूप हैं।
इनके ललाट पर लाल रंग की दो सीधी (perpendicular) रेखाएँ नासिक के ऊपर की ओर अर्धचन्द्राकार बनाती हुई मिलती हैं। उनके बीच में एक लाल बिन्दु होता है। वे तुलसी की कण्ठी धारण करते हैं। श्रीमद्भागवत की वल्लभाचार्यकृत सुबोधिनी टीका इन लोगों का प्रामाणिक ग्रन्थ है। इस मत के अनुयायियों को अपने जीवन-काल में कम-से-कम एक बार पवित्र नाथद्वारा की यात्रा अवश्य करनी चाहिए।
चैतन्य-सम्प्रदाय
इस मत का बंगाल तथा उड़ीसा में अधिक प्रचार-प्रसार है। इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है, का जन्म १४८५ ईसवी में हुआ था। लोग उन्हें कृष्ण भगवान् का अवतार मानते हैं। चौबीस वर्ष की आयु में संन्यास-ग्रहण के पश्चात् वे जगन्नाथपुरी चले गये जहाँ उन्होंने वैष्णव-मत का उपदेश दिया।
चैतन्यमतावलम्बी भगवान् कृष्ण की उपास इस प्सम पुरुष के रूप में करते हैं। इस मत के द्वार सभी जातियों के लिए खुले हुए हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी भक्त जैम निरन्तर भगवान् कृष्ण के नाम का जप करते रहते हैं।
कृष्णदासकृत चैतन्य-चरितामृत एक बृहद ग्रन्थ है। इसमें चैतन्य तथा उनके प्रमुख शिष्यों से सम्बन्धित कथाएँ प्रस्तुत की गयी हैं तथा इस मत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी किया गया है। इसकी रचना बंगला भाषा में की गयी है।
इस मत के अनुयायी वैष्णव ललाट के नीचे की ओर चन्दन अथवा गोपीचन्दन की दो श्वेत तथा सीधी (perpendicular) रेखाओं वाला तिलक लगाते हैं जो उनकी नासिका के ऊपर से आता हुआ इसके अग्रभाग तक चला जाता है। ये लोग तुलसी के छोटे-छोटे मनकों की तीन लड़ी वाली छोटी कण्ठी धारण करते हैं।
निम्बार्क-सम्प्रदाय
इस मत के प्रवर्तक निम्बार्क अथवा निम्बादित्य थे। उनका मूल नाम भास्कर आचार्य था। उन्हें सूर्य भगवान् का अवतार माना जाता है। इनके अनुयायी कृष्ण और राधा के युगल रूप की उपासना करते हैं। इनका प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ श्रीमद्भागवतपुराण है।
निम्बार्कमतावलम्बी पीत चन्दन की दो सीधी (perpendicular) रेखाएँ केश-मूल के नीचे भौंहों के निकट मोड़ दे कर मिलाते हुए तिलक लगाते हैं। इसे भगवान् के पदचिह्नों का प्रतीक माना जाता है।
निम्बार्क-सम्प्रदायी अथवा निमावत समस्त उत्तरी भारत में पाये जाते हैं। मथुरा में इनकी संख्या बहुत अधिक है। बंगाल के वैष्णव-सम्प्रदायों में से इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है।
माध्व-सम्प्रदाय
माध्व-सम्प्रदाय के लोग वैष्णव होते हैं और ब्रह्म-सम्प्रदायी के नाम से जाने जाते हैं। इस मत के संस्थापक मध्वाचार्य थे। उन्हें आनन्दतीर्थ तथा पूर्णप्रज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म १२०० ईसवी में हुआ था। वे शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धान्त अद्वैत-मत के प्रबल विरोधी थे। उन्हें वायु देवता का अवतार माना जाता है। उन्होंने उडीपी में एक मन्दिर का निर्माण कराया तथा भगवान् कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठित की थी।
माध्व-सम्प्रदाय के गुरु ब्राह्मण और संन्यासी होते हैं। इसके अनुयायी अपने अक्ष तथा कन्धों पर विष्णु का प्रतीक चिह्न धारण करते हैं। इसके चित्रांकन के भलते तम लोहे का उपयोग किया जाता है। उनका तिलक गोपीचन्दन की दो सीधी रेखामा बत होता है जो जासिका के ऊपर जा कर मिल जाता है। उस पर ये लोग भगवान कृ पर चढ़ायी हुई अगरबत्ती की भस्म से एक काली रेखा बनाते हैं जो हल्दी से बनाये हुए, गोल चिह्न में समाप्त होती है।
माध्यमतानुयायी दो उप-सम्प्रदायों में विभाजित हैं जिन्हें व्यासकूट तथा दासकूट कहा जाता है। इनकी संख्या कर्नाटक में अधिक है।
सत्य, शास्त्राध्ययन, उदारता, दया, आस्था तथा अनसूया इनकी आचार संहिता है। वे अपनी सन्तान का नामकरण विष्णु के नाम पर करते हैं और उनके शरीर पर उनके प्रतीकों को चित्रांकित करते हैं। वे मन, वचन और कर्म से सगुणों का अभ्यास करते हैं।
राधावल्लभ-सम्प्रदाय
राधावल्लभ-सम्प्रदाय के अनुयायी भगवान् कृष्ण की उपासना राधा के वल्लभ या प्रियतम के रूप में करते हैं। इस सम्प्रदाय के संस्थापक हरिवंश थे। सेवा सखी बाणी में इनके विचारों, इनकी परम्पराओं तथा मान्यताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है।
चरणदासी, दादूपन्थी, हरिचन्दी, कबीरपन्थी, खाकी, मलूकदासी, मीराबाई के इति निष्ठावान् जन, माधवपन्थी, रैदासी, सेनापन्थी, सखी-सम्प्रदाय के अनुयायी और सदमापन्थी ये सभी वैष्णव-मत के अन्तर्गत आते हैं।
शैव
दक्षिण के स्मार्त ब्राह्मण
तमिलनाडु के शैव ब्राह्मण अपने नाम के आगे अय्यर शब्द लगाते हैं। इन लोंगों को स्मार्त कहा जाता है। ये लोग अपने ललाट पर विभूति या पवित्र भस्म की तीन सीधी रेखाओं का तिलक लगाते हैं। ये सभी भगवान् शिव के उपासक हैं। इनके विभिन्न सम्प्रदाय निम्नवत् हैं :
(१) वडमा : वड देश वडमा, चोल देश वडमा तथा इंजि वडमा।
(२) बृहत्चरणम् : मलैनाट्टु बृहत्चरणम्, पलमनेरी बृहत्वरणम्, मिलघु बृहत्चरणम् तथा
कण्ड्रामानिक्क बृहत्चरणम्।
(३) वातिमार।
(४) अष्ट सहस्रम्।
(५) चोलिया जिन्हें पाण्डिमार भी कहा जाता है और जो तिरुचेन्दूर के निवासी हैं।
(६) गुरुक्कल : यह वडमाओं का ही एक उप-सम्प्रदाय है; किन्तु यह मान्यता प्राप्त नहीं है।
उनका कर्तव्य मन्दिरों में जा कर उपासना करना है। तमिलनाडु के दक्षिणी जनपदों में इन्हें पट्टर नाम से भी जाना जाता है। ये लोग अर्चकों से भिन्न होते हैं। अर्चक उपर्युक्त उप-सम्प्रदायों में से किसी भी उप-सम्प्रदाय के हो सकते हैं। वे गुरुकल अथवा पट्टरों के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में लगे परिवारों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। गुरुक्कल शब्द केवल शैवों के लिए ही व्यवहृत होता है, जब कि पट्टर और अर्चक शब्द वैष्णवों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं।
केरल के शैव ब्राह्मण
(१) नम्बूद्री, (२) मूज और (३) एमब्रान्तिरी।
बंगाल के शैव ब्राह्मण
(१) चक्रवर्ती, (२) चुन्दर, (३) राय,
(४) गांगुली, (५) चौधरी, ६) विश्वास,
(७) बागची, (८) मजूमदार और (९) भट्टाचार्य।
कर्नाटक के शैव ब्राह्मण
(१) स्मार्त, (२) हविगा, (३) कोटा, (४) शिवली, (५) तन्त्री, (६) काड़ों और (७) पाड्या।
तेलुगु स्मार्त
(१) मुरुकिनाडु, (२) वेलनाडु, (३) करणकम्मलु,
(४) पुदुरु द्राविड़ी, (५) तेलहन्यम्, (६) कोनसीमा द्राविड़ी और
(७) आरुवेल नियोगी।
लिंगायत
इन्हें वीर शैव कहा जाता है। ये कर्नाटक में पाये जाते हैं। ये एक छोटे रजत-पात्र में शिवलिंग रख कर उसे कण्ठ में धारण करते हैं।
अन्य शैव-सम्प्रदाय
आकाशमुखी, गुदारा, जंगम, करालिंगी, नखी, रुखर, सुखर, ऊर्ध्वबाहु तथा उकारा-ये सभी शैव-सम्प्रदाय के अन्तर्गत आते हैं।
शाक्त
शाक्त जगज्जननी देवी के उपासक हैं। दक्षिणी, वामी, कंचेलिया और करारी-ये सभी शाक्त-सम्प्रदाय हैं।
कुछ अन्य सम्प्रदाय
सौर सूर्य की, गाणपत्य गणेश की तथा कौमार स्कन्द की उपासना करते हैं। नायुडू, कम्म नायुडू, चेट्टी, मुदलियार, गाउण्डर, पिल्लई, नायर, नायनार और रेही दक्षिण भारत के अब्राह्मण हैं।
सात वर्गों में विभक्त नानकशाही (उदासी, गंजबख्शी, रामरावी, सूत्रशाही, गोविन्दसिंही, निर्मला, नागा), बाबा लाली, प्राणनाथी, साधु, सतनामी एवं शिवनारायणी-ये कुछ अन्य सम्प्रदाय हैं।
आर्यसमाजी तथा ब्रह्मसमाजी
स्वामी दयानन्द सरस्वती आर्य-समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म १८२४ में काठियावाड़ में हुआ था। यह समाज धार्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित एक सामाजिक सस्था है। गुरुकुलों, स्कूलों तथा पाठशालाओं की स्थापना में इसकी विशेष रुचि रहती है। आर्य-समाज की शुद्धि-सभा आर्येतर लोगों को आर्य-धर्म में दीक्षित करती है।
ब्रह्म-समाज की स्थापना मूलतः राजा राममोहन राय ने उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में की थी। ब्रह्मसमाजी मूर्तिपूजक नहीं होते। केशवचन्द्र सेन ने १८६० ईसवी में ब्रा-समाज को एक नया मोड़ दिया। अब ब्रह्म-समाज की दो शाखाएँ हो गयी हैं। प्रथम राजा राममोहन राय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करती है जिसे आदि ब्रा-समाज कहते हैं। दूसरी शाखा को साधारण ब्रह्म-समाज कहा जाता है। यह केशवचन्द्र सेन के सिद्धान्तों के अनुरूप तथा कुछ आधुनिक है। इसके अनुयायी बंगाल में पाये जाते हैं।
साधु तथा संन्यासी
प्राचीन ऋषियों, द्रष्टाऔं, सन्तों, परमहंस संन्यासियों तथा साधुओं को प्रणाम। ये लोग दिव्य ज्ञान तथा सम्यक् बुद्धि के आगार एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में संसार के भाग्य के नियामक हैं।
प्रत्येक धर्म में एक ऐसे वर्ग की व्यवस्था है जो चिन्तन और ध्यान का एकान्त तपस्वी जीवन व्यतीत करता है। इन्हें बौद्धों में भिक्षु, मुसलमानों में फकीर, सूफियों मैं सूफी फकीर और ईसाइयों में फादर तथा रेवेरेण्ड कहा जाता है। यदि आप किसी धर्म के मानचित्र से इन वैखानसों अथवा संन्यासियों या विरक्त तथा दिव्य ध्यान का जीवन बेरातीत करने वालों का अभिलोपन कर दें, तो उस धर्म की गरिमा पूर्णतः नष्ट हो जायेगी। यही वे लोग हैं जो संसार के धर्मों का रक्षण-पोषण तथा दुःखी एवं शोकाकुल गृहस्थों को सान्त्वना प्रदान करते हैं। ये लोग आत्मज्ञान, स्वर्गिक शान्ति तथा दिय ज्ञान के अग्रदूत और अध्यात्म-विज्ञान तथा औपनिषद् ज्ञान के प्रचारक-प्रसारक होते हैं। ये रोगियों का रोग निवारण करते, निराश्रितों को सान्त्वना प्रदान करते तथा रोग-शय्या पर पड़े रोगियों की परिचर्या करते हैं। ये वेदान्त-ज्ञान तथा 'तत्त्वमसि' महावाक्य के निहितार्थ को समझा कर निराश व्यक्तियों को आशा, हताश जनों को प्रफुल्लता, निर्बलों को बल एवं कायरों को साहस प्रदान करते हैं।
दशनामी संन्यासी
सनक, सनन्दन, सनत्कुमार तथा सनत्सुजात भगवान् ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इन्होंने प्रवृत्ति-मार्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया तथा निवृत्ति-मार्ग अंगीका किया। ये चारों कुमार संन्यास-मार्ग के पथ-प्रदर्शक पुरोधा थे। श्री दत्तात्रेय भी मौलिक संन्यासियों में थे। आधुनिक युग के सभी संन्यासी इन चारों कुमारों, दत्तात्रेय एवं शंकराचार्य के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं।
श्री शंकराचार्य को भगवान् शिव का अवतार माना जाता है। वे केवलाद्वैत के प्रख्यात प्रतिपादक थे और उन्होंने श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी तथा बदरीनारायण-धाम के मार्ग में हिमालय-स्थित जोशीमठ में एक-एक मठ की स्थापना की थी।
सुरेश्वर, पद्मपाद, हस्तामलक एवं तोटक-ये चारों श्री शंकराचार्य के संन्यासी शिष्य थे। सुरेश्वर, पद्मपाद, हस्तामलक एवं तोटक क्रमशः श्रृंगेरीमठ, पुरीमठ, द्वारकामठ तथा जोशीमठ के प्रभारी थे। श्री शंकर तथा सुरेश्वराचार्य के आध्यालिक उत्तराधिकारी श्रृंगेरीमठ के संन्यासियों के सरस्वती, पुरी तथा भारती-तीन नाम, द्वारकामठ के संन्यासियों के तीर्थ तथा आश्रम-दो नाम: पुरीमठ के संन्यासियों के वन तथा अरण्य-दो नाम ; जोशीमठ के के सन्यासियों के गिरि, पर्वत तथा सागर तीन नाम होते हैं।
दशनामी भगवान् शिव अथवा भगवान् विष्णु की उपासना एवं निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं। हाथों में दसह धारण करने वाले दण्डी संन्यासी शांकर परम्परा से सम्बद्ध हैं। परमहंस संन्यासी दण्ड ग्रहण नहीं करते हैं। वे परिव्राजकों की भांति स्वछन्द विचरण करते हैं। अवधूत नग्न संन्यासी होते हैं। वे नितान्त अपरिग्रही होते हैं।
रामकृष्ण मिशन के संन्यासी श्री शंकर की परम्परा से सम्बन्धित हैं। वे अपना नाम पुरी रखते हैं।
इनके अतिरिक्त निरंजनी अखाड़ा तथा जूना अखाड़ा जैसे अखाड़ों के अखाड़ा संन्यासी भी होते हैं जो शांकरमतावलम्बी होते हैं। इनकी गणना दशनामियों में की जाती है। ये केवल उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं।
ऋषिकेश तथा हरिद्वार संन्यासियों के उपनिवेशवत् हैं। वाराणसी भी संन्यासियों का प्रमुख गढ़ है।
शैव
दक्षिण भारत के तमिल संन्यासी कोवीलूर मठ तथा धर्मपुरम् अधिनम से सम्बन्धित हैं। शांकर-मत से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। वे शैव होते हैं।
नागा
नागाओं की गणना शैव-संन्यासियों में की जाती है। ये नग्न रहते हैं। ये अपने पूरे शरीर पर भस्म रमाते और दाढ़ी तथा जटा रखते हैं।
उदासी
गुरुनानक के पन्थ के तपस्वियों को उदासी कहा जाता है। ये संन्यासियों और बैरागियों के समकक्ष होते हैं। सांसारिक विषय-वासना के प्रति उदासीन रहने के कारण इहें उदासी कहा जाता है।
वैरागी
जो विषयासक्ति के भावातिरेक से रहित है, वह वैरागी है। वैरागी वैष्णव होते हैं। हे भगवान् राम, सीता और हनुमान् की उपासना तथा तुलसीदास-रचित 'रामचरितमानस' का पाठ करते हैं। रामानन्दी-सम्प्रदाय के भिक्षाटन करने वाले हैं। वैरागियों की इस परम्परा का प्रारम्भ शिष्य श्री आनन्द ने किया था।
रामसनेही
इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक रामचरन का जन्म राजस्थान में जयपुर के निकट एक गाँव में सन् १७१८ ईसवी में हुआ था। रामसनेही-मत के भिक्षाटनकर्मी सन्त विदेश गाँव मोहिनी-इन दो वर्गों में विभाजित हैं। विदेही नम रहते हैं, जब कि मोहिनी से गौरिक सूती वस्त्र धारण करते हैं। इनका मठ राजस्थान के शाहपुर में है। रोमिसनेही-सम्प्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी मेवाड़ तथा अलवर में पाये जाते हैं। के मुम्बई, गुजरात, सूरत, पूना, अहदाबाद, हैदराबाद और वाराणसी में भी मिलते हैं।
कबीरपन्थी
कबीरपन्थी सन्त कबीर के अनुयायी हैं। ये समस्त उत्तर तथा मध्य भारत में बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं। इस पन्थ की बारह शाखाएँ हैं। वाराणसी-स्थित कबीरचौरा में कबीरपन्थियों का एक बहुत बड़ा मठ है। धर्मदास कबीरदास के प्रमुढ शिष्य थे। इस पन्थ के अनुयायियों से मन, वचन और कर्म से गुरु-भक्ति की अपेक की जाती है। इन्हें सत्यवादी, दयालु, अहिंसावादी और एकान्तवासी होना चाहिए। कबीर के पुत्र कमाल के अनुयायी योगाभ्यास करते हैं।
दादूपन्थी
दादू-पन्थ वैष्णव सम्प्रदायों के अन्तर्गत ही एक पन्थ है। इस पन्थ के गुरु दादू एक कबीरपन्थी गुरु के शिष्य थे। इनके अनुयायी भगवान् राम के उपासक हैं।
अहमदाबाद में जन्म-ग्रहण करने वाले दादू जाति के धुनिया थे। इन्हें १६०० ईसवी के आस-पास का माना जाता है। दादूपन्थी विरक्त, नागा तथा विस्तरधारी-इन तीन वर्गों में विभाजित हैं। विरक्त मुण्डित-शीश होते हैं और अपने पास केवल एक वस्त्र तथा एक जल-पात्र रखते हैं। नागा लोग सशस्त्र होते हैं औ उन्हें सैनिक माना जाता है। विस्तरधारी गृहस्थ का सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।
दादूपन्थी मारवाड़ तथा अजमेर में बहुत अधिक संख्या में हैं। इनकी उपासमा का प्रमुख स्थान सम्भर तथा जयपुर के निकट नरैना में है। इनके धर्मग्रन्थों में कही है। पद सन्निविष्ट हैं।
गोरखपन्थी
गोरखनाथ कबीर के समकालीन थे। उनको भगवान् शिव का अवतार माना जाता है। वे अपने को रोज्दनाथ का पुत्र और आदिनाथ का पौत्र करतार माना जालना-स्थित गोरखपुर में गोरखनाथ का एक मन्दिर है। भर्तृहरि गोरखनाथ के शिष्य थे।
गोरक्ष-शतक, गोरक्ष-कल्प तथा गोरक्षनामा गोरखनाथ द्वारा संस्कृत में लिखित ग्रन्थ हैं।
गोरखनाथ के अनुयायियों को सामान्यतः कनफटा भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि दीक्षा ग्रहण के अवसर पर इनके कान में छेद कर उनमें कुण्डल पहना दिये जाते हैं। गोरखपन्थी भगवान् शिव की उपासना करते हैं।
निम्बार्क-सम्प्रदायी एवं रामानुज-सम्प्रदायी
निम्बार्क-सम्प्रदाय के साधु वैष्णव होते हैं। रामानुज-सम्प्रदाय के संन्यासी तरिक वस्त्र, शिखा, यज्ञोपवीत तथा त्रिदण्ड धारण करते हैं। इनकी संख्या इस समय नगण्य है।
परिणामी-सम्प्रदाय
इप्त सम्प्रदाय के संस्थापक श्री पीरननाथ का जन्म काठियावाड़-स्थित राजकोट जनपद के अन्तर्गत जामनगर में १६७५ ईसवी में हुआ था। वे राजा जामदास के दीवान थे। इस मत के अनुयायी अहिंसा, सत्य तथा दया का अनुपालन करते हैं। ये हिन्दी भाषा में रचित कुल जाम स्वरूप या आत्मबोध नामक पवित्र ग्रन्थ का पाठ करते हैं जिसमें श्री पीरननाथ के उपदेश संकलित हैं। इसमें १८,००० चौपाइयाँ हैं। ये बाल कृष्ण की उपासना करते हैं।
इस मत के अनुयायी अधिकांशतः पंजाब, गुजरात, असम, नेपाल तथा मुम्बई में पाये जाते हैं। इनके दो मठ हैं-एक जामनगर में और दूसरा पन्ना में।
दशम अध्याय
हिन्दू पौराणिकी तथा प्रतीक
हिन्दू पौराणिकी
पौराणिकी प्रत्येक धर्म का एक अभिन्न अंग है। यह दर्शन का मूर्त रूप है। वस्तुतः पौराणिकी एक ऐसा विज्ञान है जो प्राचीनकालीन, विशेषतः आदिकालीम कथाओं का अन्वीक्षण करता है। यह पाठकों को नैतिक निर्देशों एवं सटीक दृटान्तों द्वारा प्रबुद्ध कर उन्हें पूर्णत्व या उच्चतर आदशों की सम्प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करता है। अमूर्त उपदेशों एवं सूक्ष्म विचारों को कथाओं, दृष्टान्तों, जनश्रुतियों, अन्योक्तियों तथा आख्यानों में परिणत कर सामान्य जन के लिए अत्यन्त रुचिकर तथा प्रभावप्रद बनाया जा सकता है। हिन्दू-धर्म के उदात्त तथा अमूर्त दार्शनिक विचार एवं आदर्श प्रभावोत्पादक कथाओं का रूप ग्रहण कर मर्मस्पर्शी हो जाते हैं।
पौराणिकी तथा इतिहास
सभी धर्मों के अपने-अपने पुराण हैं जिनमें कुछ इतिहास का भी पुट होता है। वस्तुतः पुराण तथा इतिहास का सूक्ष्म भेद-दर्शन कठिन है। यदि कोई ईसाई उठ कर कहने लगे, "हमारे पैगम्बर ने अमुक-अमुक चमत्कारपूर्ण कृत्य किये हैं, तो इसके उत्तर में अन्य लोग कह उठेंगे, "यह तो गल्प मात्र है। हमारे पैगम्बरों ने तो इससे भी अधिक चमत्कारपूर्ण कृत्य किये हैं जो यथार्थतः ऐतिहासिक हैं।" वस्तुतः इन दोनों के सूक्ष्म अन्तर को बता पाना नितान्त दुष्कर है।
अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए हिन्दुओं के अवतारवाद का सिद्धान कपोलकल्पित और गौपूजा अन्धविश्वास है। शुद्ध-हृदय भक्तों को मुग्ध करने वाली तथा भाव-समाधि में प्रविष्ट करा देने वाली भगवान् कृष्ण की सुन्दर प्रतिमा कुछ अन्य धर्मावलम्बियों की दृष्टि में विकराल ही प्रतीत होगी। ईसाइयों, यहूदियों तथा अन्य धर्मानुयायियों के अपने पृथक् पृथक् अन्धविश्वास तथा मिथक हैं जो उनके लिए पूर्णतः ऐतिहासिक हैं। वस्तुतः पौराणिक कथाएँ काल्पनिक न हो कर सत्य के भावनात्मक प्रस्तुतिकरण की एक विधा हैं।
दर्शन, पौराणिकी तथा कर्मकाण्ड
दर्शन, पौराणिकी तथा कर्मकाण्ड प्रत्येक धर्म के ये तीन अंग होते हैं। दर्शन धर्म का सारतत्व है। यह इसके मूलभूत सिद्धान्तों, लक्ष्यों और इसा होते हैं। दर्शन साधनों का प्रतिपादन करता दर्शन पुराण महापुरुयों या लोकोतर प्राणिधीर के कर्मकाण्ड दर्शन को और अधिक मूर्त रूप प्रदान करता है जिससे यह सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य हो सके। कर्मकाण्ड धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित अर्थ करते हैं।
पुराण विभिन्न मिथकों के पुंज हैं। इनके विश्वोत्पत्ति-मीमांसा-विषयक मिथक अत्यन्त रोचक हैं। हिन्दू-त्योहारों के अवसर पर पुराणों के कुछ अंग आज भी अभिनीत किये जाते हैं जिसके फलस्वरूप जनमानस उदात्त विचारों तथा आज भी परिपूरित हो कर आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त होता है।
पौराणिकी का अध्ययन और इसकी उपयोगिता
हिन्दू-धर्म की प्राचीन पौराणिकी में महान् सत्य सन्निहित हैं। पुराणों के आवरण में आवेष्टित होने से ही कोई वस्तु उपेक्षणीय नहीं हो सकती। तर्क मत कीजिए। मौन रहिए। पुराणों के अध्ययन में बुद्धि का प्रयोग कम कीजिए। यह एक प्रतिबन्धक तत्त्व है। यह आपको भ्रम में डाल देगा। अहंकार और दम्भ का परित्याग कीजिए। कल्पना के लिए प्रेम-भाव का अभ्यास कीजिए। मुक्त-हृदय हो कर शिशु की तरह बैठिए। आप पुराणों द्वारा अनावृत-अभिव्यक्त सत्य को हृदयंगम कर लेंगे। पुराणों के प्रणेताओं तथा ऋषियों की मार्मिक भावनाओं से आप परिचित हो जायेंगे। अब आपको वास्तव में पुराणों में आनन्द आयेगा।
आप मानचित्रों की सहायता से भूगोल का अध्ययन करते हैं। वस्तुतः मानचित्रों में कोई देश नहीं होता; किन्तु इनसे विभिन्न देशों के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो बाता है। मिथकों के सम्बन्ध में भी यही बात है। इनके माध्यम से आपको सूक्ष्म आध्यात्मिक सत्यों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
पौराणिकी के अध्ययन से आपको चरित्र-निर्माण तथा आदर्श जीवन यापन के लिए पर्याप्त शिक्षा मिलेगी। आपके जीवन, आचरण तथा चरित्र को एक नयी दिशा प्रदान करने के लिए श्रीराम, श्रीकृष्ण, भीष्म, नल, हरिश्चन्द्र, लक्ष्मण, भरत, हनुमान बुधिटिर, अर्जुन, सीता, सावित्री, दमयन्ती, राधा आदि के जीवन-वृत्त आध्यात्मिक प्रेोणा के महान् स्रोत हैं। किंकर्तव्यविमूढ़ता की स्थिति में जब आपको करणीय-अकरणीय का ज्ञान नहीं रह जाता, तब पुराणों के अध्ययन से आपको अपनी समस्याओं का यथार्थ समाधान प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि पौराणिकी की कुछ अपनी उपयोगिताएँ, तथा उपलब्धियाँ हैं जो शिक्षाप्रद आख्यानों तथा प्रबोधक कथोपकथनों के माध्यम से वेदों की अमूर्त तथा सूक्ष्म शिक्षाओं को अन्तर्तम में अंकित कर देती हैं जिसके फलस्वरूप मनुष्य के लिए दिव्य जीवन यापन, पूर्णत्व, मुक्ति तथा अमरत्व के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं।
हिन्दू-प्रतीक
बाह्य प्रतीकों की आवश्यकता तथा उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्यक् दृष्टिकोण से देखने पर आपको ज्ञात हो जायेगा कि आपके भौतिक सक्का आध्यात्मिक जीवन में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। यद्यपि वे बहुत है साधारण तथा महत्त्वहीन प्रतीत होते हैं; पर वास्तव में वे अत्यधिक विज्ञानसम्मत तथा सार्थक हैं।
तिलक-एक शुभ चिह्न
तिलक एक शुभ चिह्न है। ललाट पर चन्दन, विभूति या कुंकुम का तिलक लगाया जाता है। शिव, विष्णु तथा देवी के भक्त अपने ललाट पर क्रमशः विभूति, चन्दन तथा कुंकुम का तिलक लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार तिलक-शून्य ललाट पतिहीना स्त्री, जप-काल का दुर्बोध मन्त्र, पावन पुरुषों के सम्मुख अविनत शीश, दया-शून्य हृदय, कूप-रहित भवन, मन्दिर-विहीन ग्राम, नदी-शून्य देश नेतृत्व-विहीन समाज, दान-विरहित धन, शिष्य-हीन गुरु, न्याय-शून्य देश, योब मन्त्री-रहित राजा, पति की अवज्ञा करने वाली पत्नी, जल-शून्य कूप, गन्ध-होन पुष्प, अपवित्र आत्मा, अवर्षण-ग्रस्त खेत, अस्पष्ट बुद्धि, गुरु को ईश्वर-तुल्य र मानने वाला शिष्य, अस्वस्थ शरीर, विशुद्धता-विहीन आचार, मैत्री-विहीन तर, सत्य से असम्पृक्त वाणी, सदाचार-शून्य देश, पारिश्रमिक-रहित श्रम, त्याग-पहिल संन्यास, तीर्थाटन में असंलग्न पैर, विवेकहीन निश्चय, धार-शून्य छुरा, दुग्धहीना ग तथा तीक्ष्णता-रहित भाला- ये सभी निन्दनीय हैं। इनका अस्तित्व नाम मात्र के लिए ही है। इस दृष्टिकोण से आप तिलक अथवा पवित्र चिह्न के महत्त्व को भली विधि समझ सकते हैं।
तिलक भूमध्य अर्थात आज्ञाचक्र पर लगाया जाता है । इसका प्रभाव अत्यन्त शीतल होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभावप्रद होने के अतिरिक्त चन्दन में औषधीय गुण भी होते हैं। जब आप ध्यान के लिए मन को आज्ञाचक्र पर स्थिर करते है, तब इस प्रक्रिया से उत्पन्न ताप को चन्दन प्रभाव-शून्य कर देता है। तिलक उस बिन्द की ओर संकेत करता है जहाँ ज्ञान-चक्षु खुलता है। भगवान् शिव के भ्रमध्य में एक तृतीय नेत्र है जिसके खलने पर तीनों लोक भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब जीव का तृतीय नेत्र खुलता है तब उसके आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक क्लेश-त्रय, संचित प्रारब्ध तथा आगामी कर्म-त्रय एवं पूर्वजन्मकृत सम्पूर्ण पापों का आत्यन्तिक शमन हो जाता है। तिलक लगाते समय आप कल्पना करते हैं- "मैं द्वैत भावों से युक्त अद्वितीय ब्रह्म हूँ। मेरा प्रज्ञाचक्षु शीघ्र खुल जाये।" तिलक लगाते समय आपके में इस विचार का होना आवश्यक है।
तिलक लगाने की विविध विधियाँ हैं। शैव पवित्र भस्म की तीन सीधी रेखाओं का त्रिपुण्ड लगाते हैं। वैष्णव ललाट पर तिलक धारण करते हैं और प्रार्थना करते "हे प्रभु! सत्त्व, रजस् तथा तमस् के बन्धनों से युक्त त्रिगुणात्मिका माया के दुष्प्रभाव से मेरी रक्षा करो।" कुछ वैष्णव एक ही अधोमुखी रेखा का तिलक लगाते हैं। वस्तुतः वैष्णवों तथा शैवों के तिलक लगाने की विधियों में ही अन्तर होता है। इनका निहितार्थ तो एक ही है।
शिखा : इसकी उपयोगिता तथा अर्थवत्ता
ब्राह्मण तथा अन्य जातियाँ चोटी अथवा शिखा धारण करती हैं। आज की तरह प्राचीन काल में शिखा इतनी छोटी नहीं होती थी। यह मस्तिष्क को पूर्णतः आवृत किये रहती थी। लोग इसकी वृद्धि में बाधक नहीं होते थे। वे शिखा को कभी नहीं काटते थे। यह आकस्मिक आघातों से मस्तिष्क की रक्षा करते हुए इसे शीतलता प्रदान करती है। इससे शिर सूर्य के ताप से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हो पाता। शिखा के अभाव में छतरी आदि का प्रयोग आवश्यक हो गया है।
शिखा-धारण के मूल में वैज्ञानिक तथा धार्मिक-दोनों दृष्टिकोण निहित हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान शिखा-बन्ध के पश्चात् ही करना चाहिए। केवल दाह-संस्कार तथा श्राद्धकर्म के अवसर पर ही सिखा को खुली तथा केश-राशि को अस्त-व्यस्त रखा जाता है। अस्त-व्यस्त केश-राशि अपशकुन की द्योतिका है। ऐसा केवल अत्यन्त शोक तथा विपत्ति के अवसरों पर ही किया जाता है। कौरव-सभा में शासन द्वारा चीर-हरण के अवसर पर द्रौपदी ने शपथ ग्रहण की थी कि वह जब तक अपने अपमान का समुचित प्रतिशोध नहीं ले लेती, तब तक वह मुक्त-केशी ही रहेगी। देवशरथ से उनके प्रियपात्र राम के लिए अनिष्टकर दो वरदान माँगने के लिए, कैकेयी दुसर केशी हो कर कोप- भवन में जा बैठी थी। खली गिजा के साथ शुभ कार्य कभी मीरा सम्पन्न नहीं किये जाते। आजकल बहुत कम लोग शिखा रखते हैं। पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण की धुन में महिलाएँ भी इसके महत्व के प्रति उदासीन हो गयी है। मस्तिष्क के संवेदनशील अंग तथा केन्द्रीय स्नायु-संस्थान पर शिखा का प्रभाव अत्यन्त हितकर होता है।
यज्ञोपवीत का निहितार्थ
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य यज्ञोपवीत धारण करते हैं। हिन्दुओं में यज्ञोपवीत-संस्कार एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। किसी शुभ दिन पर पाँच से आठ वर्ष की आयु के अन्तर्गत आने वाले ब्राह्मण-बालकों को यज्ञोपवीत धारण का दिया जाता है। इसके पश्चात् वे गायत्री मन्त्र के जप के अधिकारी हो जाते हैं। ब्राह्मण इस अनुष्ठान के पश्चात् ही वास्तविक ब्राह्मण हो । पाता है। कहा जाता है- "जन्मना जायते शूद्रः, कर्मणा जायते द्विजः" अर्थात् मनुष्य जन्म से शूद्र तथा को अर्थात् यज्ञोपवीत-धारण से द्विज हो जाता है। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म कहते हैं। अतः ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है।
यज्ञोपवीत में तीन धागे होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को मनसा-वाचा-कर्मणा ब्रह्मचारी होना चाहिए। यज्ञोपवीत का प्रत्येक सूत्र एक-एक कर अर्थात् ऋक्, यजु और साम का एवं एक-एक देव अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का द्योतन करता है। इनके बीच की ग्रन्थि निर्गुण ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करती है यज्ञोपवीत के सूत्र-त्रय त्रिगुणात्मिक माया के तीनों गुणों-सत्त्व, रजस् तथा तमस्-का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब कि इनकी ग्रन्थि से माया के नियन्त्रक ईश का बोध होता है। जो लोग त्रिकाल सन्ध्या के समय गायत्री मन्त्र का जप करते हु ब्रह्मग्रन्थि को पकड़ कर ईश्वर की उपासना करते हैं, उन्हें असीम शक्ति तथा ओज की। सम्प्राप्ति होती है। पुरातन काल में ब्रह्मग्रन्थि को पकड़ कर गायत्री की उपासना करने वाले साधक को वरदान तथा शाप की शक्ति प्राप्त हो जाया करती थी। आधुनिक शिक्षित बुद्धिवादी वर्ग पवित्र यज्ञोपवीत की शक्ति तथा सन्ध्योपासना के महत्व नितान्त अपरिचित हो चुका है। यही कारण है कि ये लोग इसके प्रति उदासीन हो यो। हैं। ईश्वरोपासना का नियमित जीवन व्यतीत करने वाले ब्राह्मण के लिए यज्ञापयोग में महान शक्ति निहित रहती है। इस पवित्र सूत्र की शक्ति से क्षत्रियों तथा वैश्यों को भी शक्ति, यश तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है।
विवाह के अवसर पर गृहस्थ एक अतिरिक्त यज्ञोपवीत धारण करता है; किन्तु ब्रह्मचारी के लिए केवल एक ही यज्ञोपवीत का विधान है। विवाह के समय अतिरिक्त सोपवीत धारण जीवन-साथी के मंगलार्थ किया जाता है। यज्ञोपवीत को शरीर पर सदैव धारण किये रहना चाहिए। इसे शरीर से उतार कर या धोबी के यहाँ भेज कर इक्षालित करवाना निषिद्ध माना गया है। कुछ लोगों को यज्ञोपवीत धारण कर कार्यालय जाने में लज्जा का अनुभव होता है। अतः ये लोग इसे घर पर ही छोड़ जाते है। कितने अज्ञ हैं ये!
शिखासूत्रादि हिन्दू-जाति के बाह्य चिह्न हैं। पवित्रता, आत्मसंयम, अहिंसा, धैर्व तथा मैत्री हिन्दू-धर्म के अन्तरंग लक्षण हैं।
आचमन तथा प्रोक्षण
प्रभु का नाम-स्मरण करते हुए तीन बार जल-ग्रहण को आचमन कहते हैं। जब स्नान करना सम्भव न हो, तब शरीर-शुद्धि के लिए इस पर तीन बार जल छिड़कने को प्रोक्षण कहते हैं। इससे शरीर बाह्य तथा आन्तरिक-दोनों रूपों से शुद्ध हो जाता है। जल पीते समय निम्नांकित मन्त्र का जप किया जाता है-"अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः तथा गोविन्दाय नमः ।" तत्पश्चात् शरीर के विभिन्न अवयवों-नेत्र, कर्ण, मुख, नाभि, शिर आदि का स्पर्श करते हुए भगवान् के विभिन्न नामों-केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, पद्मनाभ, दामोदर आदि का जप किया जाता है। नित्यकर्मों से निवृत्ति के उपरान्त भोजनपूर्व या भोजनोपरान्त, सड़क पर टहलने तथा स्नान के उपरान्त आचमन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इससे आपको प्रभु की उपस्थिति का यथासम्भव भान होता रहता है। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक अनुष्ठान तथा प्रत्येक प्रतीक का एक गहन आध्यात्मिक महत्व है। इससे आप रजस् तथा तमस् से ग्रस्त अपनी मानसिकता को सत्त्वोन्मुख कर सकते हैं। इससे आपको भगवत्स्मरण के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होते रहते हैं।
भगवान्, अतिथि तथा पंच-प्राणों को अन्नार्पण
भोजन के पूर्व स्थान को पवित्र कर वहाँ आसन रखा जाता है। तत्पश्चात् पत्तल पर भोजन के व्यंजन परसे जाते हैं। भोजन के पूर्व कुछ वैदिक मन्त्रों का जप करते हुए पलाल के चतुर्दिक् थोड़ा जल छिड़क दिया जाता है। इससे भोजन पवित्र हो जाता है। इसके बाद थोड़ा जल पीते हैं। भोजन के पूर्व अल्प मात्रा में जल-ग्रहण वैज्ञानिक तथा औषधीय दृष्टिकोण से अत्यन्त लाभप्रद होता है। इस प्रकार 'ॐ प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा तथा अन्त में ब्राह्मणे स्वाहा मन्त्रोच्चारण के साथ पंच-प्राणों तथा हृदयस्थ ब्रह्म को भोजन अर्पित किया जाता है। आप इस अर्पण के महत्त्व पर तो विचार कीजिए। भोजन करने वाला अपने लिए भोजन नहीं करता। भौतिक शरीर भोजन करने वाला नहीं होता। भोजन ग्रहण करने वाले तो वस्तुतः पंच-प्राण ही हैं। इस प्रकार भोजन को भी योग या यज्ञ के रूप में परिणत किया जा सकता है।
भोजन ग्रहण करने के पूर्व इसे भगवान् को अर्पित करना चाहिए। उस समय मन में यह भाव होना चाहिए-"त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये" अर्थात् गोविन्द ! तुम्हारी वस्तु तुम्हीं को अर्पित कर रहा हूँ। हिन्दुओं में यह परम्परा रही है कि भोजन के पूर्व यदि कोई घर पर आ जाता है, तो उसे भोजन कराया जाता है। अतिथि ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। श्रुति कहती है-"अतिथि देवो भव।"
घण्टी, दीप, धूप, कर्पूर तथा चन्दन
बाह्य कोलाहल से अप्रभावित रहने तथा मन को स्थिर तथा अन्तर्मुखी करने के लिए मन्दिरों में पूजा के समय घण्टियाँ बजायी जाती हैं।
देवता की आरती भी उतारी जाती है जो इस तथ्य की परिचायक है कि देवता ज्योति-स्वरूप है। वह पूर्ण प्रकाश है। भक्त कहता है- "तुम ब्रह्माण्ड के स्वयं-प्रकाश हो। सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि में जो ज्योति है, वह तुम्हारी ही है। अपने दिव्य प्रकाश से मेरे अन्तर के अन्धकार को दूर करो। मेरी प्रज्ञा प्रकाशवती हो।" आरती उतारने का निहितार्थ यही है।
देवता के सम्मुख धूप जलायी जाती है जिससे मन्दिर का कक्ष पूर्णतः धूमादित हो उठता है। धूप का धुआँ रोगाणु-नाशक होता है। धूपाग्नि से इस सत्य की ओर संकेत होता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और उसकी जीवन्त सर्वव्यापकता से अखिल विश्व ओत-प्रोत है। धूप जलाने का प्रयोजन इसी तथ्य की स्मृति में निहित है। भक प्रार्थना करता है- “हे प्रभु! जो वासना तथा संस्कार-समुदाय मुझमें सुप्तावस्था में हैं। उन्हें जला कर भस्म कर दो। मुझे निष्पाप कर दो।"
कर्पूर जलाने का तात्पर्य यह है कि वैयक्तिक अहं कर्पूर की भाँति पिघल जाता है और जीवात्मा ज्योतियों की ज्योति से मिल कर तदाकार हो जाता है।
चंदन इस तथ्य का इशारा दिलाता है कि आपातकाल में मनुष्य को चन्दन की भंति र्धर्यवान होना चाहिए । किसी कठोर वस्तु पर घर्षित करने से चन्दन से सुगन्ध निकलती है । इसका लेन बनाया जाता है । अत: भक्तको कठिनाइयों से घिर जाने पर निर्थक प्रतिवाद नहीं करना चाहिए । इसके विपरीत उसे प्रयुद्धचित्त हो कर चन्दन की भांति सदाशयता का सुरभि-दान देते रहना चाहिए। इससे यह शिक्षा भी मिलती है कि उसे अपने शत्रु से घृणा नहीं करना चाहिए। यद्यपि चन्दन को घर्षित कर उसका लेप बना दिया जाता है, तथापि वह मौन रहकर वातावरण को मधुर सुगन्ध प्रदान करता रहता है । अपने शत्रु की भी किसी प्रकार की क्षति की कामना नहीं करनी चाहिए।
प्रसाद : इसकी पवित्रता तथा महिमा
प्रसाद शान्ति प्रदान करता है। यह भगवान् को निवेदित नैवेद्य है। कीर्तन, उपासना, पूजा, हवन और आरती के समय भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान् से मीठे चावल, फल, गुड़, दूध, नारियल, केले तथा इस प्रकार की अन्य सामग्रियाँ अर्पित करता है। इस नैवेद्य-निवेदन के पश्चात् परिवार के सदस्यों अथवा मन्दिर में उपस्थित लोगों में प्रसाद-वितरण किया जाता है।
पूजा में भगवान् को जल, पुष्प, चावल आदि अर्पित किये जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् तुच्छतर भेंट से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो वस्तु अपेक्षित है, वह है मात्र हार्दिकता। गीता (९/२६) में भगवान् कहते हैं:
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ।।
"जो भी भक्त मुझे श्रद्धापूर्वक पत्र, पुष्प, फल तथा जल अर्पण करता है, उसे मैं ग्रहण कर लेता हूँ; क्योंकि यह प्रेमपूर्वक अर्पित किया गया होता है।" प्रभु को केवल स्वर्ण, रजत तथा बहुमूल्य वस्त्र अर्पित करना आवश्यक नहीं है। भक्त भगवान् को जो-कुछ भी अर्पित करता है, उसे वह अपनी क्षमता तथा अपने जीवन-स्तर के अनुरूप ही अर्पित करता है। इसका तात्पर्य यही है कि संसार की सारी सम्पदा भगवान् की ही है। एक धनवान् व्यक्ति भगवान् को बहुमूल्य वस्तुएँ अर्पित करता है, निर्धनों को भोजन देता तथा रोगियों की परिचर्या करता है और ऐसा करके वह सर्वभूतों में भगवान का ही दर्शन कर रहा होता है।
पूजा बिल्वपत्र, पुष्प, तुलसी और विभूति से की जाती है और इन्हें भगवान् का प्रसाद मान कर वितरित किया जाता है। विभूति भगवान् शिव का प्रसाद है जिसे मस्तक पर धारण किया जाता है। अल्प मात्रा में इसका ग्रहण भी किया जा सकता है। कुंकुम देवी या शक्ति का प्रसाद है। इसे भूमध्य में लगाया जाता है। तुलसी भगवान् विष्णु, राम या कृष्ण का प्रसाद है। इसका सेवन करना चाहिए। पूजा तथा हवन के समय मन्त्रोच्चारण द्वारा इनमें रहस्यात्मक शक्तियों का उद्रेक होने लगता है।।
भोगार्पण के समय भक्त के मनोभाव का अत्यधिक महत्त्व है। यदि भगवान् का कोई अनन्य भक्त भगवान् को कोई वस्तु अर्पित करता है, तो इस प्रसाद के ग्रहण के फलस्वरूप नास्तिकों की मानसिकता में भी महान् परिवर्तन हो जाता है। प्रसाद के ही माध्यम से भगवत्कृपा का अवतरण होता है। नारदचरित्र पढ़िए। इससे आपको भगवान् तथा उन्नत साधकों तथा सन्तों के पवित्र प्रसाद अथवा उच्छिष्ट की गरिमा की स्पष्ट अनुभूति हो जायेगी।
पाण्डुरंग विठ्ठल ने नामदेव द्वारा अर्पित चावल आदि ग्रहण किये। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं नामदेव को भी सहभोजी बना लिया। यदि भगवान् को उत्कण्ठित हृदय से भोजन अर्पित किया जाता है, तो वे कभी-कभी सदेह उपस्थित हो कर उसे ग्रहण का लेते हैं। अन्य अवसरों पर वे अर्पित भोजन के सारतत्त्व को ग्रहण करते हैं और यह भोजन प्रसाद के रूप में यथावत् रह जाता है। महात्माओं तथा निर्धनों को भोजन कराने के पश्चात् जो शेष रह जाता है, उसको प्रसाद-रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। यज्ञानुष्ठान में सब लोगों में प्रसाद-वितरण किया जाता है। इससे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुत्रेष्ठि-यज्ञ की समाप्ति पर दशरथ को पायस से भरा एक पात्र मिला जिसे उन्होंने अपनी रानियों को दे दिया और रानियाँ उस पायस को ग्रहण का गर्भवती हो गयीं। भक्त के लिए प्रसाद पवित्रतम वस्तु है। प्रसाद ग्रहण कर मनुष्य को स्वयं को धन्य एवं सौभाग्यशाली समझना चाहिए। प्रसाद ग्रहण में किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। इस पर देश, काल तथा सामाजिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रसाद की पवित्रकारिता असन्दिग्ध है।
प्रसाद तथा चरणामृत के लाभ वर्णनातीत हैं। इनमें मानव-जीवन के दृष्टिकोर को मूलतः परिवर्तित कर देने की शक्ति निहित रहती है। इनमें रोगियों को रोग-मुक तथा मृतकों को जीवित तक कर देने की क्षमता है। हमारे देश की पावन धरती पर ऐलो कई-एक घटनाएँ हो चुकी हैं जिन्हें प्रसाद की शक्ति तथा क्षमता के दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रसाद से दुःखों की निवृत्ति तथा पापों का शमन होताहै। यह शोक, दुःख तथा चिन्ता की रामबाण औषधि है। इस कथन की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धाहीन व्यक्ति के लिए यह अधिक प्रभावाप्रद नहीं है।
आधुनिक शिक्षा पद्धति तथा संस्कृति में पले-परपे लोग प्रसाद की महिमा को विस्मृत कर चुके हैं। अधिकांश अंगरेजी पदे-लिखे लोग महात्माओं द्वारा प्रदत्त प्रसाद को कोई महत्व नहीं देते। यह एक भयंकर भूल है। प्रसाद में पवित्रीकरण की महान शक्ति निहित है। पाश्चात्य जीवन पद्धति के अन्तर्गत पालित-पोषित होने के कारण उनका चिन्तन पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप हो गया है। वे प्राचीन काल के ऋषियों की सन्तान की मनीषा से अपरिचित हो गये हैं। आप एक सप्ताह के लिए वृन्दावन वा अयोध्या या वाराणसी या पण्डरपुर में चले जाइए। आपको प्रसाद के चमत्कारिक प्रभाव तथा इसकी महिमा की स्पष्ट अनुभूति हो जायेगी। इससे कई असाध्य रोगों का निवारण हो जाता है। अनेक निष्कपट समर्पित साधकों को प्रसाद से ही आध्यात्यिका अनुभवों की प्राप्ति हो जाती है। प्रसाद एक अचूक औषधि तथा अध्यात्म-सुधा है। यह परमात्मा का आशीर्वाद तथा सर्व दुःखों की रामबाण औषधि है। प्रसाद शक्ति तथा दिव्यता का मूर्त रूप है। प्रसाद से भक्ति संवर्धित, पुष्ट एवं तेजोमयी होती है। इसका ग्रहण विश्वासपूर्वक करना चाहिए।
जप-माला
मनकों की संख्या का निहितार्थ
सामान्यतः जप के लिए प्रयुक्त होने वाली माला में १०८ मनके होते हैं। मनुष्य प्रतिदिन २१,६०० बार साँस लेता है। यदि मनुष्य २०० माला का जप करता है, तो जप की संख्या २१,६०० हो जाती है। वह प्रति साँस एक बार जप करता है। इसका अर्थ होता है कि वह दिन-भर हरि-स्मरण करता है। १०८ मनकों की विभाजित संख्या भी मनकों की संख्या हो सकती है। इससे गणना में कोई अन्तर नहीं आता। मेरु (मरकों के बीच वाला मनका) से यह ज्ञात हो जाता है कि आपने १०८ बार जप कर लिया है। यह इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि आपकी उँगलियाँ जब भी कभी मेरु का स्पर्श करती हैं, आप आध्यात्मिक पथ पर एक पग आगे निकल चुके होते हैं और आपकी एक बाधा नष्ट हो चुकी होती है। इस प्रकार आपके अज्ञान के एक अंश की निवृत्ति हो जाती है। माला एक ऐसा प्रेरणाप्रद उपकरण है जो आपको आप के लिए उत्प्रेरित करता रहता है। प्रार्थना करते समय मुसलमानों के हाथ में भी बत्ता रहती है। वे मनके फेरते रहते हैं तथा अल्लाह का नाम जपते रहते हैं। ईसाइयों के लिए उनकी अपनी प्रार्थनाएँ होती हैं।
रक्षा-स्तोत्र
जप तथा ध्यान पर बैठने से पूर्व सामान्यत: रक्षा-स्तोत्र की आवृत्ति की जाती है। इसमें कहा जाता है "परमात्मा मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में अवस्थित होकर है। मेरी रक्षा करें।" शरीर के विभिन्न अवयवों के पृथक् पृथक् नामों का स्मरण किया जाता है तथा प्रत्येक अंग के रक्षार्थ भगवान् के विशेष नाम का उच्चारण किया जाता है । अंगन्यास और करन्यास का भी यही प्रभाव होता है। ये दुष्टात्माओं के अनिष्टकर प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यदि धारणा तथा ध्यान में कोई अन्तराय आ जाता है,तो यह उसका निराकरण कर देता है। यह ऐसी प्रार्थना है जिससे जप तथा ध्यान में आने वाली विघ्न-बाधाओं का निराकरण हो जाता है।
गेरुआ वस्त्र तथा मुण्डित शिर
त्याग के प्रतीक
संन्यासी का गेरुआ वस्त्र इस तथ्य का द्योतक है कि वह अग्नि की भाँति पवित्र है। इच्छाओं तथा वासनाओं के कल्मष से मुक्त वह तपे हुए स्वर्ण की भाँति चमकता है। काषाय वस्त्र पवित्रता का सूचक है। इससे शुचिता का द्योतन होता है। निवृत्तिमागी साधक के लिए यह सहायक सिद्ध होता है। वह अशुभ कर्मों के प्रति विरक्त हो जाता है। यह वस्त्र उसे स्मरण दिलाता है कि वह सांसारिक सुखोपभोग का अधिकारी नहीं है। धीरे-धीरे उसमें स्वभावगत परिवर्तन होने लगता है। रंगीन वस्त्र संन्यासी की पहचान का बाह्य प्रतीक है।
संन्यासी पूर्णतः मुण्डित-शीश होता है। इससे उसकी सुन्दरता जाती रहती है। उसे सुगन्धित तैलादि द्वारा अपनी केश-राशि के सौन्दर्य-रक्षण की चिन्ता नहीं रहती। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह बाह्य सौन्दर्य के सभी रूपों से विरत हो कर आत्मा में स्थित हो गया है जो सौन्दर्यों का सौन्दर्य है। मुण्डन से इस तथ्य का संकेत प्राप्त होता है कि संसार के लिए उसका अस्तित्व शून्यवत् रह गया है। उसे किसी ऐन्द्रिय विषय की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः मुण्डित-शीश पूर्ण अनासक्ति की मनःस्थिति एवं जागतिक सुखों के प्रति विरति का बाह्य प्रतीक मात्र है। संन्यास-ग्रहण के समय वह शिखा-विहीन भी हो जाता है। यह इस बात का द्योतक है कि वह विभिन नित्य-नैमित्तिक कर्मों के बन्धन से मुक्त हो चुका है और कि ये सारे कर्म वैराग्य की अग्नि में जल कर भस्म हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त मुण्डित-शीश यायावर-जीवन के लिए सुविधाजनक भी होता है। केश-राशि उसके इच्छानुसार स्नान में बाधक सिद्ध होगी। मुण्डन से वह कई असुविधाओं से मुक्त हो जायेगा। उसका जो समय बालों को सुखाने तथा सजाने-सँवारने में व्यतीत होता, उसका उपयोग वह प्रार्थना तथा ध्यान में कर सकता है।
निष्कर्ष
वेद तथा उपनिषद् परम सत्य का वर्णन अनौपचारिक विधि से इसके विशुद्ध एवं नए रूप में करते हैं; किन्तु इतिहास, पुराण तथा आगम ऐतिहासिक कथाओं एवं पुराकथाशास्त्रीय आख्यानों के माध्यम से उसे एक वैयक्तिक संस्पर्श प्रदान कर देते हैं।
बाह्य प्रतीकों की उपेक्षा मत कीजिए। वैदिक प्रथाओं तथा विधि-निषेधों का अनुसन्धानात्मक अध्ययन कीजिए। आपको इनमें से प्रत्येक में आश्चर्यजनक तथा अमूल्य रत्न प्राप्त होंगे। उनका अनुसरण करने से उनकी उपयोगिता तथा कार्यक्षमता ज्ञात हो जायेगी।
आप सब धर्म के मार्ग पर चलते हुए इसी जन्म में कैवल्य प्राप्त करें!
एकादश अध्याय
हिन्दू-दर्शन-१
(षड्-दर्शन)
दर्शन : इसका उद्भव तथा इसकी सीमाएँ
दर्शन धर्म का बौद्धिक अथवा युक्तिपरक पक्ष है। भारत में इसे धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है। यह परम सत्य तथा चरम सत्ता के स्वरूप का तर्कसम्पत अनुसन्धान है। यह जीवन की सूक्ष्म तथा गहन समस्याओं का स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करता है और क्लेश तथा मृत्यु से मुक्ति तथा अमरता एवं शाश्वत आनन्द की प्रारि की दिशा में हमारा पथ-प्रदर्शन करता है।
दर्शन की मूल स्थापनाएँ मनुष्य की व्यावहारिक आवश्यकताओं में निहित हैं। चिन्तन के क्षणों में मनुष्य लोकोत्तर विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उसमें मृत्यु, अमरत्व, आत्मा, स्रष्टा तथा सृष्टि के रहस्योद्घाटन की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। उसके इस अभियान में दर्शन उसका सहायक सिद्ध होता है। दर्शन मनुष्य की उत्तरोत्तर विकासशील चेतना की आत्माभिव्यक्ति है। दार्शनिक इस चेतना को शब्दबद्ध करते हैं। महान् सर्जनात्मक चिन्तक तथा दार्शनिक प्रत्येक युग में हुए हैं। वे मनुष्य को उन्नत तथा प्रेरित करते रहते हैं।
मनुष्य के मन में दर्शन-सम्बन्धी कुछ निश्चित प्रश्न उठा करते हैं। यह संसार है क्या? इसका कोई प्रयोजन भी है? यह सत्य-स्वरूप है या प्रतीतिमात्र ? क्या इस विश्व का कोई स्रष्टा या शास्ता है? यदि कोई इसका स्रष्टा है, तो उसका स्वरूप क्या है ? मनुष्य और स्रष्टा का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है, क्या जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति का कोई मार्ग भी है? क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसे निर्वैयक्तिक एवं निरुपाधिक अथवा निरपेक्ष कहा जा सके ? यदि ऐसी कोई वस्तु है, तो उसका मूलभूत स्वभाव क्या है? मनुष्य के बन्धन का कारण क्या है? उसकी तात्त्विक प्रकृति क्या है? वह सर्वोच आत्मा का एक अंशमात्र है या उससे अभिन्न है? वैयक्तिक या सगुण ईश्वर एवं निर्गुण या निर्वैयक्तिक निरपेक्ष ब्रह्म में अन्तर क्या है? इस संसार का उद्गम क्या है? पदार्थ और मन क्या है? जीवात्मा क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? इन समस्याओं के समाधान की खोज ही दर्शन है। यह इन समस्त समस्याओं का सम्यक् समाधान प्रस्तुत करता है।
मृत्यु : दर्शन का प्रारम्भ-बिन्दु
मृत्यु-सम्बन्धी विचार सदैव से ही धर्म तथा धार्मिक जीवन की सर्वाधिक प्रभावपूर्ण अभिप्रेरक शक्ति रहा है। मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है। मृत्यु उसके लिए, अभीप्सित घटना नहीं है। वह अमरत्व चाहता है। दर्शन का प्रारम्भ-बिन्दु यही है। दर्शन इसका अन्वेषण और अनुसन्धान करता है। इसकी निर्भीक उद्घोषणा यही है। मनुष्य! मृत्यु से भयभीत न हो। तुम्हारे लिए एक नित्य-धाम की व्यवस्था है जिसे ब्रह्म कहते हैं। वह तुम्हारा आत्मस्वरूप है जो तुम्हारी हृदय-गुहा में निवास करता है। तुम पवित्र हृदय से उस अनघ, नित्य एवं अविकारी आत्मा का ध्यान करो। तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा।" मृत्यु संसार की नश्वरता तथा एक चरम सत्ता के अस्तित्व का संकेत-चिह्न है।
दर्शन के विभिन्न मतवाद (Schools)
मनुष्य तथा ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्ध का स्पष्ट बोध दर्शनशास्त्र के विद्यार्थियों तथा सभी साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। संसार के दार्शनिकों, पैगम्बरों, सन्तों, चिन्तकों, आचार्यों तथा धर्मगुरुओं ने ईश्वर से मनुष्य तथा विश्व के सम्बन्ध की व्याख्या के प्रयत्न किये हैं। दर्शनशास्त्र के विभिन्न मतवादों तथा विभिन्न धार्मिक मतों का प्रादुर्भाव विभिन्न दार्शनिकों की विविध व्याख्याओं के आधार पर ही हुआ है।
दर्शनशास्त्र तथा अन्तः प्रज्ञा
दर्शनशास्त्र आपको शाश्वत आनन्द के परिमण्डल के द्वार तक तो पहुँचा सकता है; किन्तु उसके लिए आपको उस परिमण्डल में प्रविष्ट करा देना असम्भव है। नित्य-सुख तथा अनिर्वचनीय महिमा की उस धरती पर पैर रखने के लिए अन्तःप्रज्ञा अथवा लोकोत्तर अनुभूति आवश्यक है।
हिन्दू-दर्शन निराधार परिकल्पना या अर्थहीन अनुमान मात्र नहीं है। यह उदात्त, भव्य, अद्वितीय तथा व्यवस्थित है। यह रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक अनुभवों अथवा अपरोक्षानुभूति पर अधिष्ठित है। जिन द्रष्टाओं, साधु-सन्तों तथा ऋषियों ने परम सत्य का अव्यवहित तथा सहजानुभूत साक्षात्कार किया था, वे ही भारत की विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के प्रवर्तक हैं। दर्शनशास्त्र के विभिन्न मतों में से सभी प्रत्यक्षतः या परोक्षतः:. श्रुति अथवा वेदों पर आश्रित है। जो लोग उपनिवदों का सुविचारित अध्ययन करते हैं, उन लोगों को श्रुतियों के अपौरुषेय उदघाटन तथा दर्शनशास्त्र के निष्कर्षो की पारस्परिक समस्वरता का सम्यक् ज्ञान हो जाता है।
भारतीय दर्शन की शास्त्रसम्मत तथा शास्त्रविरुद्ध शाखाएँ
षड-दर्शन भारतीय दर्शन की छह शास्त्रसम्मत शाखाएँ हैं। न्याय, वैशिषेक, साहित्य, योग, पूर्वमीमांसा तथा उत्तर मीमांसा या वेदांत परम सत्य के दर्शन के छह शास्वानुभोदित मार्ग हैं। दर्शन की शास्त्रसम्मत शाखाएँ बेदों की प्रामाणिकता है विश्वास करती हैं, जब कि इसकी शाखविरुद्ध शाखाएँ, वेदों की प्रामाणिकता से विश्वास नहीं करतीं। ये छह शास्त्रविरुद्ध मत निम्नवत् हैं
१. चार्वाक का पदार्थवादी मत।
२. जैन-मत।
३. बौद्धों का वैभाषिक मत।
४. बौद्धों का सौत्रान्तिक मत।
५. बौद्धों का योगाचार मत।
६. बौद्धों का शून्यवादी या माध्यमिक मत।
षड्-दर्शन अथवा छह शास्त्रसम्मत मतवाद
षड्-दर्शनों का वेदों से प्रत्यक्ष उद्भव हुआ है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है दृश्य या देखना। प्रत्येक दर्शन सत्य के अन्वीक्षण का एक मार्ग या इसके प्रति एक दृष्टिकोण है।
गौतम ऋषि ने न्याय के सिद्धान्तों या भारतीय तर्कशास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया और कणाद ने वैशेषिक सूत्रों की रचना की। कपिल मुनि सांख्य-पद्धति के प्रणेता थे और सर्वप्रथम पतंजलि महर्षि ने योग-प्रणाली को एक सुसम्बद्ध रूप दे का योग-सूत्रों की रचना की। इनका योग-दर्शन राजयोग पर एक प्रख्यात पाठ्य-पुस्तक है। व्यास के शिष्य जैमिनि ने वेदों के कर्मकाण्डीय भाग पर आधारित मीमांसा-सूत्रों की रचना की। बादरायण ने अपने प्रख्यात वेदान्त-सूत्रों अथवा ब्रह्म-सूत्रों की रचना की जो उपनिषदों के उपदेशों का प्रतिपादन करते हैं। वेदान्त के विभिन्न मतों ने अपने दर्शनों को इसी आधार-भूमि पर अवस्थित किया है।
मार्ग अनेक; गन्तव्य एक
षड़-दर्शन एक नगर में पहुँचने के छह विभिन्न मार्गों के सदृश हैं। आप बम्बई रेलगाड़ी या वायुयान या बस या अन्य किसी वाहन से जा सकते हैं। इसी प्रकार आप योग या वेदान्त या अन्य किसी भी मार्ग से अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। मनुष्य को उसके लक्ष्य तक ले जाने के लिए उसके स्वभाव एवं उसकी क्षमता तथा मानसिक शक्ति के अनुरूप विभिन्न विधियों या मागों की व्यवस्था है; किन्तु इन सभी भागों का लक्ष्य एक ही है और वह है जीवात्मा तथा परमात्मा के सायुज्य के माध्यम से अज्ञान तथा तज्जनित क्लेशों की निवृत्ति एवं स्वातन्त्र्य, पूर्णत्व, अमरत्व तथा नित्य-सुख की सम्प्राप्ति।
हिन्दू-धर्म के किसी भी विद्यार्थी को उक्त छह दार्शनिक मतों के अभिलाक्षणिक भेदों को स्पष्ट करने वाले सिद्धान्तों की अभिज्ञता के बिना अपने ज्ञानार्जन से सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अधिक प्रबुद्ध अध्येता को उन मूल सूत्रों का अध्ययन करना चाहिए जिनमें प्रत्येक मत के सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है। इन छह दार्शनिक मतों के अध्ययन से आपकी बुद्धि सुतीक्ष्ण तथा आपका ज्ञान विशद होगा। इससे आपका परम सत्य-सम्बन्धी ज्ञान अधिक व्यापक होगा। प्रत्येक मत आध्यात्मिक सोपान का एक चरण है।
षड्दर्शनों का पारस्परिक सम्बन्ध
उक्त छह मत तीन वर्गों में विभाजित हैं : (१) न्याय तथा वैशेषिक, (२) सांख्य तथा योग, और (३) मीमांसा तथा वेदान्त। वैशेषिक तथा योग क्रमशः न्याय और सांख्य के सम्पूरक हैं। वेदान्त सांख्य का अभिवर्धन एवं इसकी आपूर्ति है। इसकी ज्ञान-प्राप्ति के लिए व्याकरण, मीमांसा, न्याय और सांख्य का अध्ययन आवश्यक है। न्याय के अध्ययन से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और उसके फलस्वरूप जिज्ञासु वेदान्त के ज्ञान-ग्रहण में समर्थ होता है। न्याय सभी दार्शनिक अनुसन्धानों के लिए पूर्वापेक्षित है।
वैशेषिक-दर्शन का आजकल अधिक महत्त्व नहीं रह गया है; किन्तु न्याय की जनप्रियता में कोई व्यवधान नहीं आया है। सांख्य-मत की जीवन्तता समाप्तप्राय है और योग के व्यावहारिक पक्ष का अभ्यास कुछ गिने-चुने लोगों तक ही सीमित रह गया है। आजकल इन सभी मतों में वेदान्त को सर्वाधिक जनप्रियता प्राप्त है।
न्याय तथा वैशेषिक आपके समक्ष आनुभविक जगत् की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ये संसार की सभी वस्तुओं को कुछ विशिष्ट पदार्थों के अन्तर्गत वर्गीकृत कर देते हैं। वे इस तथ्य की व्याख्या करते हैं कि ईश्वर ने अणु-परमाणुओं से इस भौतिक जगत् की सृष्टि किस प्रकार की है। वे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारा जगत प्रदर्शन करते हैं। सांख्य आपको हिन्दू-मनोविज्ञान का गहन ज्ञान प्राप्त कराता है। कपिल मुनि मनोविज्ञान के आदि प्रणेता थे। चित्त-वृत्ति-निरोध तथा ध्यान योग के विषय हैं। योग मन तथा इन्द्रियों के अनुशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह चित्त की स्थिरता एवं एकाग्रता तथा निर्विकल्प-समाधि में प्रविष्टि में आपके लिए सहायक सिद्ध होता है। पूर्वमीमांसा वेदों के कर्मकाण्ड से तथा उत्तरमीमांसा वेदों के ज्ञानकाण्ड से सम्बन्धित हैं। उत्तरमीमांसा को वेदान्त-दर्शन भी कहते हैं। यह हिन्दू धर्म की आधारशिला है। वेदान्त-दर्शन ब्रह्म के स्वरूप की विशद व्याख्या एवं जीवात्मा तथा परमात्मा की तात्विक अभिन्नता का प्रतिपादन करता है। यह अविद्या के निवारण तथा जीव की ब्रह्म से सायुज्य-प्राप्ति की विधियों का विवेचन करता है। न्याय तथा सांख्य अज्ञान को क्रमशः मिथ्या ज्ञान और अविवेक कहते हैं। यथार्थ तथा अयथार्थ में अभेद-दर्शन अविवेक है। वेदान्त इसे अविद्या कहता है। ज्ञान द्वारा इसका उन्मूलन प्रत्येक दर्शन का लक्ष्य है। मनुष्य को अविद्या की निवृत्ति के पश्चात् ही शाश्वत आनन्द तथा अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है।
न्याय तथा वैशेषिक के अध्ययन से मनुष्य संसार की भौतिक संरचना की ज्ञान-प्राप्ति एवं भ्रान्ति-दर्शन के लिए बुद्धि के प्रयोग में सक्षम होता है। सांख्य के अध्ययन से वह प्रकृति के विकास-क्रम से परिचित होता है और योग के अध्ययन तथा अभ्यास से उसे आत्म-निग्रह एवं मन तथा इन्द्रियों पर स्वामित्व की प्राप्ति होती है। वेदान्त के अध्ययन से मनुष्य अविद्या का निराकरण कर आध्यात्मिकता या दिव्य महिमा के उच्चतम सोपान पर आरूढ़ हो जाता है और उसको चरम सत्ता के साथ अपने तादात्म्य का बोध हो जाता है।
वेदान्त : दर्शन-शास्त्र की सर्वाधिक सन्तोषप्रद शाखा
न्याय, वैशेषिक, सांख्य तथा योग के कुछ सिद्धान्त वेद-विरोधी हैं। वस्तुतः वे मत वेदों पर सतही रूप से ही आश्रित हैं। न्याय तथा वैशेषिक वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं; किन्तु मुख्य रूप से वे मानवीय विवेक-बुद्धि पर ही निर्भर है। मनुष्य की बुद्धि सान्त तथा चपल होती है। इसकी अपनी सीमाएँ हैं। इसका व्यापार दिक्, काल तथा कारण-कार्य की सीमाओं के अन्तर्गत ही सम्पन्न होता है। अतः इसके निष्कर्ष निर्दोष नहीं हो सकते। इससे लोकोत्तर या अनुभवातीत विषयों का समाधान असम्भव है। एकमात्र वेद ही निर्मान्त तथा प्रामाणिक हैं। इनमें दृष्टाओं तथा ऋषियों के अन्तःप्रज्ञात्मक अनुभव समाविष्ट हैं जो ब्रह्मज्ञानियों के अनुभव के अनुरूप हैं।
दर्शन की सर्वाधिक सन्तोषजनक प्रणाली वेदान्त ही है। इसका उद्भव उपनिषदों से हुआ है। यह दर्शन की समस्त शाखाओं का अप्रवतीं है। मीमांसा में कर्मकाण्ड पर अत्यधिक बल दिया है। इसके अनुसार वेदों में एकमात्र कर्म का ही प्रतिपादन किया गया है। उपासना या ज्ञान इसके उपांग मात्र हैं। वेदान्त इस अवधारणा का खण्डन करता है। इसके अनुसार ज्ञान मुख्य तथा कर्म एवं उपासना गौण हैं। इन्हें ज्ञान का उपांग मात्र कहा जा सकता है। कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो परिष्कृत विषयोपभोग का एक अस्थायी स्थान है। शाश्वत आनन्द तथा अमरत्व प्रदान करने में अक्षम कर्म जन्म-मरण के चक्र को उन्मूलित नहीं कर सकता।
शंकराचार्य के युग में दर्शनशास्त्र की सभी छह शाखाएँ पुष्पित-पल्लवित हो रही थी। अतः उन्हें अपने सिद्धान्त केवलाद्वैत के प्रतिपादन के लिए अन्य मतों का खण्डन काना पड़ा। किन्तु आजकल सांख्य तथा वैशेषिक आदि का अस्तित्व केवल नाम मात्र को ही रह गया है। किन्तु आज भी कुछ हिन्दू-उपदेशक, संन्यासी तथा मण्डलेश्वर पुरातन दार्शनिक मतों का खण्डन कर अद्वैत-मत को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह उनकी भूल है। इस युग में भौतिकवाद, अज्ञेयवाद, निरीश्वरवाद एवं विज्ञान का खण्डन कर वेदान्त का प्रतिष्ठापन करना चाहिए।
न्याय
भूमिका
दर्शन की न्याय-प्रणाली के प्रवर्तक ऋषि गौतम को प्रणाम !
न्याय तथा हिन्दू-तर्कशास्त्र के प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। इन्हें अक्षपाद तथा दीर्घतमस् के नाम से भी जाना जाता है। न्याय तथा वैशेषिक-दर्शन विश्लेषणात्मक हैं। न्याय शब्द किसी विषय में प्रवेश या इसके विश्लेषणात्मक अनुसन्धान का अभिव्यंजक है। इस विश्लेषण के निहितार्थ के अनुसार न्याय शब्द सांख्य के संश्लेषण का सर्वथा विपरीतार्थी है। न्याय को कभी-कभी तर्कविद्या या वादविद्या भी कहा बोता है। तर्क न्याय का विशिष्ट लक्षण है।
न्याय औपचारिक तर्कशास्त्र मात्र न हो कर एक समग्र ज्ञानशास्त्र है। सामान्य जन के मतानुसार न्याय का सम्बन्ध मुख्यतः तर्कशास्त्र से है; किन्तु तर्कशास्त्र इसका एक प्रकरण या अंग मात्र है। न्याय का प्रयोजन तर्कयुक्त प्रमाण पर अधिष्ठित सिद्धाको एक माध्यम से ज्ञान के विषय का आलोचनात्मक परीक्षण है। न्याय दार्शनिक समस्याओं पर आलोचनात्मक विधि से विचार करता है। इसमें मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, तत्त्वशास्त्र तथा धर्मविज्ञान-सम्बन्धी विचार-विमर्श का समावेश है।
न्याय : दार्शनिक अनुसन्धान की विधि
न्याय का अभिप्राय मानवीय ज्ञान के प्रमेय-प्रमाता के अनुसन्धान की निर्भ्रान्त पद्धति प्रस्तुत करना है जिसमें विचार-विधि तथा बुद्धि और विवेक भी सन्निहित रहते हैं। इसमें इन्द्रियों के साक्ष्य को आलोचनात्मक परिपृच्छा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। न्याय ज्ञान की यान्त्रिकता का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। न्याय तथा वैशेषिक अनुभव के लिए देश, काल, कारण, पदार्थ, मन, आत्मा तथा ज्ञान अथवा प्रमा का अन्वेषण-गवेषण कर अपने निष्कर्ष को विश्व-सम्बन्धी सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। न्याय तथा वैशेषिक एक ही इकाई के अवयव हैं। वैशेषिक न्याय का अनुपूरक है। ये समवर्गीय पद्धतियाँ हैं। ये दोनों वैयक्तिक अर्थात् सगुण ईश्वर, आत्माओं की अनेकता तथा अणुसंघात-जनित विश्व में विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों में अनेक युक्तियाँ उभयनिष्ठ हैं।
न्याय संस्कृत दार्शनिक अध्ययन का आधार है। यह समस्त सुव्यवस्थित दर्शनों की पूर्व-पीठिका है। यह दर्शन के विद्यार्थी के लिए प्रारम्भिक पाठ्य-पुस्तक है। न्याय के ज्ञान के अभाव में आप श्री व्यास कृत ब्रह्मसूत्र को नहीं समझ सकते। इसके अध्ययन से तर्कशक्ति का विकास होता है। इससे बुद्धि तीक्ष्ण तथा सूक्ष्म होती है। तीक्ष्ण तथा सूक्ष्म बुद्धि के अभाव में वेदान्त-सम्बन्धी विषयों का अनुसन्धान असम्भव है। कठोपनिषद् (१/३/१२) में आया है: "दृश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः।” अर्थात् इसे (आत्मा को) सूक्ष्म-द्रष्टा अपनी तीक्ष्ण तथा सूक्ष्म बुद्धि द्वारा देखते हैं।
गौतम का 'न्यायसूत्र' न्यायदर्शन का प्रथम ग्रन्थ है। यह इस मत का सर्वाधिक प्रख्यात ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ पर अनेक भाष्यकारों ने अनेक भाष्यों की रचना की है। दृष्टान्त के लिए वात्स्यायन कृत न्यायभाष्य, श्रीकण्ठ कृत न्यायालंकार, जयन्त कृत न्यायमंजरी, गोवर्धन कृत न्यायबोधिनी तथा वाचस्पति मिश्र कृत न्यायवार्त्तिकतात्पर्य-टीका आदि के नाम लिये जा सकते हैं।
ज्ञान
ज्ञान के लिए प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति तथा प्रमाण का चतुर्ग्यूह पूर्वपेिक्षित है। प्रमेय अर्थात् वे विषय जिनके सम्यक् ज्ञान की अपेक्षा है, उनकी संख्या बारह हे ये हैं :
(१) आत्मा, (२) शरीर, (३) इन्द्रियाँ,
(४) अर्थ, (५) बुद्धि, (६) मन,
(७) प्रवृत्ति, (८) दोष, (९) प्रेत्य-भाव,
(१०) फल, (११) दुःख और (१२) अपवर्ग।
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द-ये चार प्रमाण हैं जो सम्यक् ज्ञान के करण अथवा साधन हैं। आप्त पुरुषों के वचन भी शब्द-प्रमाण के अन्तर्गत हैं और इन्द्रिय का पदार्थ से संयोग होने पर प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है।
ईश्वर, आत्मा तथा विश्व
ईश्वर
न्याय के अनुसार मनुष्य के कर्मों से उनके फलों की उत्पत्ति होती है। इसे अदृष्ट कहते हैं और इसका निष्पादन ईश्वर के नियन्त्रण में ही होता है। ईश्वर अदृष्ट की प्रक्रिया का पर्यवेक्षक है। अदृष्ट का बुद्धिसम्मत सिद्धान्त मनुष्य की नियति का नियमन करता है और ईश्वर अदृष्ट का नियामक है। वस्तुतः ईश्वर अदृष्ट की दिशा में कोई परिवर्तन न कर इसकी प्रक्रिया में सहायता मात्र प्रदान करता है। ईश्वर मनुष्यों का कर्म-फल-दाता है। वह सर्वशक्तिमत्ता तथा सर्वज्ञता से सम्पन्न एक विशिष्ट आत्मा है। अपने इन गुणों से वह संसार का नियमन और संचालन करता है।
ईश्वर एक सगुण सत्ता है जो मिथ्या ज्ञान, अधर्म तथा प्रमाद से रहित है। वह स्रष्टा तथा एक है और नित्य-ज्ञान तथा इच्छा-क्रिया उसके गुणों से युक्त हैं। वह विभु अर्थात् सर्वव्यापी है।
आत्मा
आत्मा एक यथार्थ सत्ता है। यह एक शाश्वत सत्ता है। इच्छा, द्वेष, संकल्प, सुख, दुःख, बुद्धि और ज्ञान इसके गुण हैं। 'मैं' की अवधारणा का विषय ही आत्मा है। इसके अभाव में कोई भी संज्ञान या प्रत्यभिज्ञान सम्भव नहीं है। आत्मा के बिना नेत्र वस्त्रु-दर्शन और कान शब्द-श्रवण में असमर्थ हैं। इन्द्रियों के व्यवहार के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता होती है। वह कर्ता यह आत्मा ही है। किसी विषय के दर्शन के पश्चात् द्रष्टा का 'मैंने देखा है' यह ज्ञान शेष रह जाता है, भले ही वह व्यक्ति नेत्रहीन ही क्यों न हो गया हो। यह ज्ञान न तो इन्द्रियों का गुण है न इसके विषयों का। मन आत्मा नहीं है। यह आत्मा का साधन या करण है जिससे वह सोचता है। आत्मा कर्ता है। शरीर-पात तथा इन्द्रियों और मन से सम्बन्ध-विच्छेद के पश्चात् भी इसकी सता अक्षुण्ण रहती है। आत्माएँ बहुसंख्यक हैं।
विश्व
विश्व नित्य, अविकार्य और कारण-रहित परमाणुओं का संयोजन है। विश्व की स्वतन्त्र सत्ता है और यह विचार-सापेक्ष नहीं है। विश्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का रूपान्तरण है। न्याय नौ द्रव्यों को स्वीकृत करता है। ये नौ द्रव्य हैं-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन तथा आत्मा।
बन्धन का कारण तथा अपवर्ग के साधन
मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म तथा दुःख विश्व के संघटक तत्त्व हैं। मिथ्या ज्ञान समस्त क्लेशों तथा दुःखों का मूल है। मिथ्या ज्ञान से राग-द्वेष के दोष की तथा राग-द्वेष से शुभाशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है। शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को पुरस्कार या दण्ड-ग्रहण करने के लिए अनेक जन्म-ग्रहण करने पड़ते हैं। जन्म-मरण से दुःख प्राप्त होता है। दर्शन का लक्ष्य इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति है जो सर्वदुःखों का मूल है। मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म तथा दुःख के आनुक्रमिक तथा आत्यन्तिक निराकरण से अपवर्ग की प्राप्ति होती है।
सोलह पदार्थ
मनुष्य सोलह पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का निराकरण कर आत्यन्तिक आनन्द को प्राप्त कर सकता है। ये सोलह पदार्थ हैं-प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रह-स्थान।
प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में सर्वप्रथम संशय या भ्रम उत्पन्न होता है। इसके पश्चात् प्रयोजन अर्थात् विचार-विमर्श का अभिप्राय तथा दृष्टान्त आते हैं। सिद्धान्त अर्थात् प्रमाणित निष्कर्ष दृष्टान्त का अनुगामी है। इसके पश्चात् पंचावयव, तर्क तथा निर्णय आते हैं। तर्क शंका-निवर्तक तथा निर्णय विषय की समीचीनता के सम्बन्ध में निश्चय या निष्कर्ष है। तत्पश्चात् आता है वाद, जिसका अनुगमन करते हैं जल्प तथा वितण्डा। जल्प अपने पक्ष-समर्थन का अर्थहीन प्रयास तथा वितण्डा निरर्थक छिद्रान्वेषण है। इसके पश्चात् हेत्वाभास और निग्रह-स्थान आते हैं। हेत्वाभास में असद हेतु निहित रहता है और निग्रह स्थान-से-की- युक्ति संबंधी अक्षमता के कारण परिचर्चा का अन्त हो जाता है।
ज्ञान की प्राप्ति होने पर व्यक्ति के दोष अर्थात राग, देव तथा मोह विलिन हो जाते हैं। यहाँ द्वेष में क्रोध, ईर्ष्या, दुर्भावना तथा घृणा का, राग में कामुकता, लोभ तथा लिप्सा का एवं मोह में सन्देह, अहंकार, प्रमाद तथा मिथ्या बोध का भी समावेश हैं। मोह से राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मिध्या ज्ञान से प्रारम्भ तथा दुःख में अन्त होने वाली श्रृंखला को समाप्त करना होगा। यदि मिथ्या ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो दोष भी विलीन हो जायेंगे और यदि दोष विलीन हो जाते हैं, तो व्यक्ति प्रवृत्ति से तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाले देहान्तरण तथा दुःख से मुक्त हो जाता है।
देहान्तरण में आत्मा एक शरीर का परित्याग कर अन्य शरीर ग्रहण कर लेता है। ग्रह देहान्तरण उसके सुख-दुःख भोग का कारण है। देहान्तरण से मुक्त आत्मा सर्वदुःखों से मुक्त हो जाता है। शरीरपात तथा इसके फलस्वरूप सुख-दुःख की निवृति के पश्वात् शीघ्र ही उसे परम मुक्ति या निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है।
अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था
अपवर्ग या मोक्ष दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति है। यह क्लेश-मुक्त अवस्था है। इसमें दुःखों का ध्वंस हो चुका होता है। यह सुखोपभोग भावात्मक नहीं है। यह आत्मोन्मूलन नहीं है। यह बन्धनाश है। इक्कीस प्रकार के दुःखों की निवृत्ति ही मोक्ष है। मुक्तावस्था में मन का आत्मा से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। इस स्थिति में इच्छा, प्रवृत्ति, धर्म, अधर्म, द्वेष तथा मानसिक संस्कार आत्मा के आश्रय-स्थान नहीं रह जाते; क्योंकि मन अब सत्ता-शून्य हो चुका होता है। नैयायिकों का मोक्ष एक अर्थहीन शब्द है; क्योंकि यह नितान्त संवेदन-शून्य पाषाणवत् दुःख तथा भाव-रहित अवस्था है।
निष्कर्ष
सृष्टि का प्रारम्भ परमाणुओं के संयोजन से हुआ है। इसमें संयोग तथा वियोग निहित है। ईश्वर, परमाणु तथा नौ द्रव्य सृष्टि के कारण हैं। ईश्वर नित्य-ज्ञान-सम्पन्न है। इच्छा तथा क्रिया उसके गुण हैं। वह विभु है। जीव कर्ता तथा भोक्ता है। जीव अनेक हैं और उनमें अनेक गुण हैं। अज्ञान बन्धन का कारण तथा बन्धन इक्कीस प्रकार के दुःखों का परिणाम है। मोक्ष सर्वदुःखों से निवृत्ति है। आत्मज्ञान, जो ज्ञान के अन्य प्रकारों से भिन्न है, मोक्ष का साधन है। गौतम आरम्भवाद तथा अन्यथाख्याति के समर्थक हैं।
वैशेषिक
भूमिका
वैशेषिक-दर्शन के प्रवर्तक कणाद ऋषि को मौन प्रणाम ! कणाद ऋषि को औलूक्य और काश्यप नामों से भी जाना जाता है।
वैशेषिक-मत के नामकरण के मूल में 'विशेष' शब्द निहित है जो पदाथों के स्वभावगत पार्थक्य का द्योतक है। कणाद के सूत्रों में वैशेषिक-दर्शन का मूल-तत्त्व निहित है। इसमें जिस मुख्य विषय का निरूपण किया गया है, वह 'विशेष' है जो इस मत के प्रवर्तक द्वारा परिगणित छह पदार्थों में एक है।
न्याय तथा वैशेषिक
आत्मा के स्वभाव तथा गुण और विश्व-रचना के मूलभूत सिद्धान्तों के विषय में वैशेषिक तथा न्याय एकमत हैं। वैशेषिक न्याय का सम्पूरक है। वैशेषिक का मुख्य प्रयोजन अनुभव की व्याख्या है। पहले यह अपनी जिज्ञासाओं को पदार्थों के आधार पर अर्थात् अस्तित्ववान् वस्तुओं के समर्थन में आने वाले सामान्य गुणों का नामनिर्देशन करने की पद्धति के आधार पर क्रमबद्ध करता है। यह कुछ सामान्य अवधारणाओं का प्रतिपादन करता है जो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द-प्रमाण द्वारा ज्ञेय वस्तुओं से सम्बद्ध हैं।
कणाद के सूत्र
कणाद के वैशेषिक-सूत्र दश अध्यायों में विभाजित हैं। प्रथम अध्याय में पदार्थों के समस्त वर्ग पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय में कणाद ने द्रव्यों (substances) का अभिनिश्चयन किया है और तृतीय अध्याय में उन्होंने आत्मा तथा आन्तरिक इन्द्रिय (मन) का वर्णन किया है। चतुर्थ अध्याय में शरीर तथा उसके अवयवों की परिचर्चा है और पंचम में कर्म का प्रतिष्ठापन किया गया है। षष्ठ अध्याय में कणाद ने धर्म पर शास्त्रानुमोदित विधि से विचार किया है। सप्तम अध्याय में उन्होंने गुणों तथा समवाय का प्रतिष्ठापन और अष्टम में ज्ञान की अभिव्यक्ति, इसके स्रोत आदि का अभिनिश्चयन किया है। नवम अध्याय में उन्होंने 'विशेष' का तथा दशम में आत्ला के गुण-वैभिन्य का प्रतिपादन किया है।
प्रारम्भ में नामनिर्देशन करते हुए पदार्थों का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात् उनको परिभाषित और तत्पश्चात् उनका परीक्षण किया गया है।
यह मत मुख्यतः पदार्थों के निर्धारण से सम्बन्धित है; किन्तु कणाद इसका प्रारम्भ धर्म के अनुसन्धान से करते हैं। इसका यह कारण है कि पदार्थों के सारतत्त्व के ज्ञान के मूल में धर्म ही है। इसका प्रथम सूत्र है :
"यतोभ्युदयनिःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः।"
अर्थात् जिससे परम कल्याण अथवा मोक्ष (दुःखों की समाप्ति) की प्राप्ति होती है, वह धर्म है।
सप्त पदार्थ
पदार्थ का शाब्दिक अर्थ 'पद का अर्थ' होता है; किन्तु यहाँ इसका अभिप्राय उस द्रव्य से है, जिसकी दर्शनशास्त्र में विवेचना की गयी है। पदार्थ वह है जिसके विषय में सोचा जा सकता है (अर्थ) तथा जिसका कोई नाम (पद) है। समस्त अस्तित्ववान्, दृश्यमान, नामधारी तथा अनुभवगम्य वस्तुएँ पदार्थ हैं। पदार्थ ज्ञान का विषय होने से शेप तथा नामधारी होने से अभिधेय है। संयोजित द्रव्य पराश्रित तथा अनित्य हैं, जब कि सामान्य द्रव्य नित्य तथा स्वतन्त्र हैं।
वैशेषिक में निम्नांकित पदार्थों की परिगणना की गयी है :
(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, (४) सामान्य, (५) विशेष, (६) समवाय और (७) अभाव।
इनमें से प्रथम तीन अर्थात् द्रव्य, गुण तथा कर्म की यथार्थ या वस्तुपरक सत्ता है। अन्य तीन अर्थात् सामान्य, विशेष तथा समवाय तर्क-सिद्ध पदार्थ हैं। ये बौद्धिक विभेदीकरण-जन्य हैं। कणाद ने केवल छह पदार्थों की गणना की है; किन्तु उत्तरकालीन मनीषियों ने एक सातवें पदार्थ की भी परिगणना कर दी।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन-ये नौ द्रव्य हैं। इनमें से प्रथम चार तथा अन्तिम को परमाणु-जन्य कहा जाता है। प्रथम चार नित्य तथा अनित्य-दोनों हैं। अपने विभिन्न मिश्र रूपों में होने से ये अनित्य हैं; किन्तु अपने अन्तिम परमाणुओं (जिनमें इनका उद्गम है) के सन्दर्भ में ये नित्य हैं।
मन एक नित्य द्रव्य है। आत्मा के असदृश यह सर्वव्यापी नहीं है। यह परमाणु-जन्य है और एक समय में केवल एक ही विषय का विचार कर सकता है।"
नौ द्रव्यों में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न-ये सतरह गुण हैं। इनमें जिन सात अन्य गुणों को समाविष्ट किया जाता है, वे हैं-गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेहा संस्कार, धर्म, अधर्म तथा शब्द। इनमें से सोलह गुण अनात्म (भौतिक) द्रव्यों से सम्बद्ध हैं। शेष आठ (बुद्धि, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, धर्म तथा अघर्ष) आत्मा के गुणधर्म हैं।
तृतीय पदार्थ कर्म पाँच प्रकार का माना जाता है-उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन।
चतुर्थ पदार्थ सामान्य के दो भेद हैं-पर-अपर तथा परापर।
पंचम पदार्थ 'विशेष' प्रथम पदार्थ के नौ नित्य द्रव्यों (पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन) से सम्बन्धित है। इन सभी मैं नित्य तथा मूलभूत भेद है और ये सभी एक-दूसरे से पृथक् हैं। इस 'विशेष' के कारण ही इस दर्शन या मत को वैशेषिक कहा जाता है।
षष्ठ पदार्थ समवाय एक ही प्रकार का होता है। यह द्रव्यों तथा उनके गुणों, जाति तथा उसके व्यष्टियों एवं किसी वस्तु तथा उससे सम्बन्धित सामान्य प्रत्यय में सहवतीं होता है। यह एक यथार्थ तत्त्व माना जाता है।
सप्तम पदार्थ अभाव दो प्रकार का होता है- (१) संसर्गाभाव अर्थात् दो वस्तुओं में होने वाले संसर्ग या सम्बन्ध का निषेध अथवा अभाव। संसर्गाभाव तीन प्रकार का होता है- (अ) प्रागभाव (उत्पत्ति के पहले कारण में कार्य का अभाव), (आ) प्रध्वंसाभाव (उत्पत्ति के पीछे कारण में कार्य का अभाव) और (इ) अत्यन्ताभाव (वर्तमान, भूत तथा भविष्य-तीनों कालों में दो वस्तुओं के संसर्ग का अविद्यमान रहना); तथा (२) अन्योन्याभाव (अर्थात् एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है अर्थात् दोनों में पारस्परिक भेद है)। इन दोनों भेदों को मिलाने से अभाव चार प्रकार का हो जाता है।
पदार्थों के ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति
पदार्थ-ज्ञान अभ्युदय की प्राप्ति का साधन है। पदार्थों की एकरूपता या इनके भेद द्वारा इनके सारतत्त्व के किसी धर्म-विशेष द्वारा उत्पन्न ज्ञान का परिणाम है-निःश्रेयस ।
अदृष्ट का सिद्धान्त और इसकी अपर्याप्तता
कणाद ने अपने सूत्रों में ईश्वर का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। उनके मतानुसार, विश्व की रचना अदृष्ट का परिणाम है जो कमाँ की अलक्षित शक्ति है। वे अदृष्ट के सिद्धान्त को ही परमाणुओं तथा आत्माओं के आदि व्यापार का उदाम मानते हैं। कणाद के अनुयायी ईश्वर को जगत् का निमित कारण तथा परमाणुओं को उपादान कारण मानते हैं।
अविचारशील परमाणु इस विश्व के सुव्यवस्थित संचालन में असमर्थ हैं; क्योंकि इसके लिए उनमें अपेक्षित शक्ति तथा बुद्धि का अभाव है। परमाणुओं के कार्यों का नियमन निश्चित रूप से सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापी परमात्मा द्वारा ही होता है। अनुमान तथा धर्मग्रन्थों के कारण हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के लिए विवश हैं। जिसके कारण अदृष्ट क्रियाशील होता है, वह बुद्धि क्या है? वह बुद्धि ईश्वर है। पचमहाभूत कार्य हैं। उनका कोई ऐसा पूर्ववर्ती होना आवश्यक है जिसे इनका ज्ञान हो। वह 'पूर्ववर्ती' ईश्वर है। वेदों का कोई प्रणेता अवश्य होना चाहिए। वेदों में जो-कुछ भी है, वह निर्भान्त तथा उनका प्रणेता निश्छल है। उसके लिए सर्वज्ञ होना अनिवार्य है।
प्रलयावस्था में आत्माएँ बुद्धि-रहित हो जाती हैं। अतः वे परमाणुओं का नियन्त्रण नहीं कर सकतीं। परमाणु स्वयं गतिशील होने में असमर्थ हैं। अतः इनकी गति का कोई आदि उत्प्रेरक होना ही चाहिए। यह आदि उत्प्रेरक सृष्टिकर्ता अथवा ईश्वर है।
विश्व का परमाणुवादी सिद्धान्त
वैशेषिक-मत के अनुसार विश्व की संरचना परमाणुओं के संयोग से होती है। परमाणु असंख्य तथा नित्य हैं। अदृष्ट की शक्ति द्वारा उनका निरन्तर संयोग, विघटन तथा पुनः विघटन हुआ करता है। परमाणु को सत्, कारण-रहित तथा नित्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सूक्ष्मातिसूक्ष्म, अदृश्य, अविभाज्य, अमूर्त तथा इन्द्रियों के लिए अगोचर है। प्रत्येक परमाणु में एक 'विशेष' अथवा उसका अपना नित्य सारतत्व निहित रहता है। प्रारम्भ में परमाणुओं के संयोग से द्वयणुक की सृष्टि होती है। तीन टूवणुकों के संयोग से त्रसरेणु उत्पन्न होता है। सूर्य की किरणों में दृश्यमान एक रज-ऋण के आयतन के समान इसका उतना ही आयतन होता है कि इसे देखा जा सके।
परमाणुओं के चार वर्ग हैं-पृथ्वी के, जल के, तेज के तथा वायु के परमाणु। पृथक् पृथक् परमाणु एक-दूसरे से संयुक्त हो कर कुछ काल के उपरान्त पुनः विघटित हो जाते हैं।
'वैशेषिक-सृष्टिमीमांसा इस अर्थ में द्वैतवादी है कि इसमें नित्य-आत्माओं के साथ-साथ नित्य-परमाणुओं की सत्ता को भी मान्यता दी गयी है। इसमें आत्मा तथा पदार्थ के यथार्थ सम्बन्ध के विषय में कोई निश्चयात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।
शरीर तथा आत्मा
शरीर प्रलय के समय सूक्ष्म तथा सृष्टि के समय स्थूल हो जाता है। काल, देश एवं जन्म की परिस्थितियों, परिवार तथा जीवनावधि का निर्णायक अदृष्ट है।
वैयक्तिक आत्माएँ नित्य, अनेक, एक-दूसरे से नित्य-रूप से पृथक् तथा शरीर, इन्द्रियों एवं मन से भिन्न हैं; किन्तु इनमें बुद्धि, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, धर्म तथा अधर्म आदि गुण निवास करते हैं। ये अनन्त, सर्वव्यापी और चतुर्दिक् फैले हुए हैं। मनुष्य का आत्मा जितना न्यूयार्क में है, उतना ही बम्बई में भी है, यद्यपि वह केवल उसी स्थान पर अपने बोध, संवेदना तथा क्रिया की शक्तियों का उपयोग कर सकता है जहाँ उसका शरीर होता है। आत्मा तथा मन प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय नहीं हैं।
मोक्षावस्था में आत्मा का गुणों से आत्यन्तिक सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। इसे अपने स्वातन्त्र्य की पुनः प्राप्ति हो जाती है।
जन्म, मरण तथा मोक्ष
धर्म तथा अधर्म द्वारा आत्मा के शरीर, इन्द्रिय तथा जीवन के साथ संयोग को जन्म तथा इनके द्वारा शरीर तथा मन के वियोजन को मरण कहते हैं।
जब आत्मा शरीर से संयोजित नहीं होता तथा साथ ही, किसी सम्भाव्य (potential) शरीर की सत्ता नहीं होती एवं परिणामस्वरूप पुनर्जन्म असम्भव हो जाता है, तब यह स्थिति मोक्ष कहलाती है।
बन्धन तथा मोक्ष
आत्मा, इन्द्रिय, मन तथा विषयों के पारस्परिक सन्निकर्ष से सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं।
सुख से इच्छा उत्पन्न होती है। पुष्प-माला, चन्दन-लेप, स्त्री तथा अन्य विषयों के भोग से प्राप्त सुख से इसी प्रकार के सुख या इसकी प्राप्ति के साधनों के प्रति एक के बाद दूसरा राग उत्पन्न होता जाता है। सर्प, वृश्चिक, कण्टक या इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं से उत्पन्न दुःखों के कारण इन दुःखों या इनके कारणों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है।
निरन्तर अथवा अभ्यास-जनित विषयानुभव का मन पर एक ऐसा सशक्त संस्कार पड़ जाता है कि अपनी प्रेमिका के हृदय को विजित करने में असमर्थ प्रेमी प्रत्येक वस्तु में अपनी प्रेमिका का ही दर्शन करने लगता है। इसी प्रकार, सर्प-दंश से पीड़ित रह चुके व्यक्ति को सर्वत्र सर्प-दर्शन ही होता है।
दोष जो बन्धन के कारण हैं
राग, द्वेष तथा मोह को दोष कहा जाता है; क्योंकि वे उस कर्म के अभिप्रेरक हैं जो कर्ता को संसार के बन्धन में डाल देता है। गौतम भी कहते हैं- "दोष कर्म या जागतिक व्यापार के लिए उत्प्रेरित करता है" (न्यायसूत्र : १/१/१८)।
ज्ञान : मोक्ष का साधन
आत्मा के अन्तर्ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। इसके फलस्वरूप राग, देष, मोह तथा अन्य दोषों की निवृत्ति हो जाती है। इस स्थिति में कर्म भी समाप्त हो जाता है। अतः कर्म-जनित जन्म भी नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप जन्म के कारण उत्पन्न दुःख की भी निवृत्ति हो जाती है।
सांख्य
भूमिका
सांख्य-दर्शन के प्रवर्तक, ब्रह्मा के पुत्र तथा विष्णु के अवतार श्री कपिल मुनि को प्रणाम !
सांख्य शब्द का अर्थ है संख्या। दर्शन की इस पद्धति में जगत् के पचीस तत्त्वों की परिगणना की गयी है। अतः इसका नाम सर्वथा उपयुक्त है। सांख्य शब्द का प्रयोग विवार या आध्यात्मिक चिन्तन के सन्दर्भ में भी किया जाता है।
सांख्य-पद्धति में यथार्थरूपेण स्थित तथा विषयों एवं संवेगों में वर्गीकृत सत्ता के रूप में विश्व की विश्लेषणात्मक परिपृच्छा के दर्शन नहीं होते। यह दर्शन मूलभूत तत्व प्रकृति, जिससे अन्य समस्त जागतिक पदार्थों का प्रादुर्भाव होता है, का संस्लेषणात्मक विवेचन करता है।
सांख्य-पद्धति में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्त-वाक्य-ये तीन प्रमाण है। आम शब्द का अर्थ सम्यक् या निर्भान्त है। इसका प्रयोग वेदों या अपौरुषेय ज्ञान प्राप्त गुरुओं के लिए किया जाता है। नैयायिकों को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द, ये चार प्रमाण मान्य हैं और मीमांसक छह प्रमाणों को स्वीकार करते हैं।
पुरुष तथा प्रकृति की द्वैतवादी अवधारणा
सांख्य का अध्ययन सामान्यतः न्याय के अध्ययन के पश्चात् ही किया जाता है। दर्शन की यह एक सुन्दर पद्धति है जो पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा भी प्रशंसित है। इसका द्वैतवाद अन्य दर्शनों के द्वैतवाद से अधिक सम्पुष्ट तथा स्पष्ट है। इसके मतानुसार शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति असम्भव है। यह पुरुष तथा प्रकृति की यथार्थ सत्ता के प्रति आस्थावान् है। पुरुष ज्ञाता तथा प्रकृति ज्ञेय है।
प्रकृति तथा पुरुष अनादि तथा अनन्त हैं। इनमें एकत्व-दर्शन जन्म-मरण का हेतु है। इनके पृथकत्व के बोध से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रकृति तथा पुरुष, दोनों सत् हैं। पुरुष असंग है। वह चेतन, विभु तथा नित्य है। प्रकृति कर्ता तथा भोक्ता है। पुरुष असंख्य हैं।
ईश्वर के प्रति अस्वीकृति
सांख्य को निरीश्वरवादी सांख्य कहा जाता है। यह नास्तिक दर्शन है। ईश्वर के प्रति इसकी आस्था नहीं है। प्रकृति द्वारा आविर्भूत सृष्टि की अपनी एक पृथक् सत्ता है जो उस पुरुष-विशेष के समस्त सम्बन्धों से स्वतन्त्र है जिसके साथ वह सम्बद्ध है। अतः सांख्यमतानुसार संसार को किसी चेतन स्रष्टा या नियन्त्रक शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।
यह एक भ्रान्त धारणा है। वेदान्त के अनुसार, प्रकृति सदैव परमात्मा के नियन्त्रण में रहती है। यह स्वयं कुछ कर पाने में असमर्थ है। यह परमात्मा की दृष्टि-परिधि से बाहर नहीं जा पाती। एकमात्र इसी के कारण उसमें गति का संचार होता है और वह सृष्टि की संरचना का प्रारम्भ करती है। प्रकृति अचेतन है। एकमात्र किसी चेतन स्रष्टा के पास ही ब्रह्माण्ड-सम्बन्धी कोई सुविचारित योजना हो सकती है। प्रकृति तो सहकारी मात्र है। यह वेदान्त का सिद्धान्त है।
विकास तथा प्रत्यावर्तन
सांख्य का सिद्धान्त विकास तथा प्रत्यावर्तन का सिद्धान्त है। कारण तथा कार्य एक ही तत्त्व की अविकसित तथा विकसित अवस्थाएँ हैं। आत्यन्तिक विनाश या प्रलय जैसी कोई स्थिति नहीं होती। प्रलय में बस इतना ही होता है कि कार्य कारण मैं विलीन हो जाता है।
शून्य से किसी भी वस्तु का आविर्भाव नहीं हो सकता। जो नहीं है, वह उस वस्तु में विकसित नहीं हो सकती, जो है। अव्यक्त रूप में जिसका अस्तित्व नहीं है, उसका प्रादुर्भाव मानव-श्रृंग की भाँति एक असम्भावना मात्र है, क्योंकि किसी वस्तु के प्रादुर्भाव के लिए किसी उपादान का होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का आविर्भाव एक ही स्थान में सर्वदा नहीं हो सकता और किसी भी वस्तु का आविर्भाव उसी वस्तु से हो सकता है जो उसको आविर्भूत करने में सक्षम हो।
जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसको किसी कर्ता द्वारा अस्तित्व प्रदान कर पाना या अभिव्यक्त कर देना असम्भव है। यदि मूँगफली में तेल नहीं है, तो उससे तेल निकालने का प्रयास निष्फल होगा। इस युक्ति से रेत या सन्तरे से भी मूँगफली का तेल निकालना असम्भव है। तेल की अभिव्यक्ति या इसका प्रादुर्भाव मूँगफली में तेल की पूर्व-सत्ता का प्रमाण है। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि इस कार्य में वह कारण पूर्व-काल में विद्यमान था जिससे इसका आविर्भाव हुआ।
कार्य में कारण की पूर्व-सत्ता का होना असन्दिग्ध है। सांख्य-दर्शन की केन्द्रस्थ विशिष्टताओं में इस सिद्धान्त की भी गणना की जाती है। कार्य वह तत्त्व है जो कारण में अव्यक्त रूप से निहित रहता है। जिस प्रकार वृक्ष बीज में अव्यक्तावस्था या प्रसुप्तावस्था में सर्वांशतः विद्यमान रहता है, उसी प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड अव्यक्त या अव्याकृत प्रकृति में विद्यमान रहता है। निसर्गतः कार्य कारण से अभिन्न है। यह अपने कारण या उपादान से भिन्न नहीं होता।
पचीस तत्त्वों का चतुर्वर्गीय विभाजन
सांख्य तत्त्वों का वर्णन उनकी अपनी-अपनी रचनात्मक क्षमता के आधार पर जाता है। ये हैं-१. प्रकृति, २. प्रकृति तथा विकृति, ३. विकृति और ४. न प्रकृति न विकृति। इस चतुर्वर्गीय विभाजन में सारे पचीस तत्त्वों का समावेश हो जाता है। प्रधान या प्रकृति विशुद्धतः प्रसवधर्मिणी है। यह सबकी मूल है। यह विकृति नहीं है। यह एक सर्वसात्यक शक्ति है जिससे वस्तुओं का आविर्भाव तथा विकास होता है। बुद्धि, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएँ-ये प्रकृति तथा विकृति, दोनों हैं। बुद्धि से अहंकार का आविर्भाव होता है, अतः बुद्धि प्रकृति है; किन्तु स्वयं प्रकृति से आविर्भूत होने के कारण यह विकृति भी है। अहंकार विकृति है; क्योंकि इसका प्रादुर्भाव बुद्धि से होता है। यह प्रकृति भी है; क्योंकि इससे पंच तन्मात्राओं का आविर्भाव होता है। अहंकार से आविर्भूत होने के कारण पंच तन्मात्राएँ विकृति हैं; किन्तु इनसे पंच महाभूतों का आविर्भाव होता है, अतः ये प्रकृति भी हैं। दश इन्द्रियाँ, मन तथा पंच महाभूत विकृति मात्र हैं। इसका कारण यह है कि इनसे किसी ऐसे तत्त्व का आविर्भाव नहीं हो सकता जो इनसे मूलतः भिन्न हो। पुरुष या आत्मा न तो प्रकृति है न विकृति। यह निर्गुण है।
सांख्य-दर्शन का प्रयोजन
इस दार्शनिक मत के अनुसन्धान का प्रयोजन आध्यात्मिक, (ज्वरादि व्याधियाँ) आधिदैविक, (विद्युत्-पात, शीत, ताप और वर्षादि) तथा आधिभौतिक (पशुओं तथा वृश्चिकादि द्वारा हुई पीड़ा) दुःखों के आत्यन्तिक उच्छेदन के साधनों की खोज है। दुःख प्रतिबन्धक होता है। इससे योग-साधना तथा मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उपस्थित होता है। कपिल मुनि द्वारा प्रदत्त पचीस तत्त्वों का ज्ञान दुःख का विनाशक है। सांख्य-दर्शन के अनुसार जिसे इन पचीस तत्त्वों का ज्ञान हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इन त्रिविध दुःखों का अत्यन्ताभाव ही जीवन का चरम लक्ष्य है।
प्रकृति
प्रकृति का अर्थ प्रधान है। यह सृष्टि का मूल तत्त्व है। इस शब्द की निष्पत्ति 'प्र' अर्थात् पूर्व तथा 'कृ' अर्थात् कृति से होती है। यह वेदान्त की माया के समकक्ष है। यह विश्व का एकमात्र मूल है। इसे प्रधान इसलिए कहा जाता है कि इसमें सारे परिणाम या सारी विकृतियाँ अव्यक्त रूप से अनुस्यूत हैं और यह विश्व तथा इसके विषयों का आदि कारण है।
प्रकृति के लक्षण
प्रधान या प्रकृति नित्य, सर्वव्यापी तथा अचल है। यह एक है और इसका कोई कारण नहीं है। यह स्वयं समस्त कार्यों का कारण है। यह स्वतन्त्र तथा अविकृत है, जब कि अन्य तत्त्व विकृति तथा परतन्त्र हैं। प्रकृति एकमात्र अपने गुणों की सक्रियता पर ही निर्भर है।
प्रकृति अचेतन है। यह एक त्रिसूत्र की भाँति है। इसके तीन गुण ही यह त्रिसूत्र हैं। यह एक निश्चेतन तत्त्व है। इसमें जो शक्ति है, वह इन गुणों के ही कारण है।
प्रकृति का रूपान्तरण
मूल पदार्थ अव्यक्त होता है। महत् अर्थात् वैश्विक चेतना प्रकति की प्रथम विकृति है। बुद्धि या महत् अहंकार के लिए प्रकृति है। अहंकार बुद्धि की विकृति है। एक ऐसी प्रकृति है। यह एक ए जिससे इन्द्रियों तथा तन्मात्राओं का आविर्भाव होता है। प्रकार इन्द्रियाँ तथा पंच तन्मात्राएँ अहंकार की विकृति हैं। स्थूल भूत पंच तन्मात्राओं की विकृति हैं।
महत्, अहंकार तथा पंच सूक्ष्म तन्मात्राओं का आविर्भाव प्रकृति से ही होता है। इस प्रकार महत् से ले कर तन्मात्राओं तक सारे तत्त्वों का आविर्भाव प्रकृति के इपान्तरण के फलस्वरूप ही होता है। इन कार्यों से कारण (प्रकृति) का अनुमान होता है। कारण अपनी सूक्ष्मता से अगोचर होता है; अतः इसका अनुमान इसके कार्यों से ही होना चाहिए।
प्रकृति का व्यापार
प्रकृति वस्तुगत सत्ता का मूलाधार है। यह अपने लिए सृष्टि नहीं रचती। सारे पदार्थ आत्मा के भोग के लिए ही होते हैं। जिस प्रकार कोई पुष्प पारदर्शी मणि-कलश के सम्पर्क में आ जाता है, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के सम्पर्क में आ कर ही सृष्टि-रचना करती है। प्रत्येक आत्मा के मोक्ष के लिए ही यह व्यापार सम्पन्न होता है। जिस प्रकार दुग्ध का कार्य बछड़े का पोषण है, उसी प्रकार प्रकृति का कार्य आत्मा को मोक्ष प्रदान करना है।
गुण
सांख्य-दर्शन के अनुसार सत्त्व, रजस् तथा तमस्, ये त्रिगुण प्रकृति के उपादान तत्व हैं। सत्त्व निर्मलता तथा प्रकाश का, रजस् आवेग, प्रवृत्ति तथा गति का और तमस् जड़ता, अन्धकार तथा निष्क्रियता का द्योतक है।
गुण का अर्थ सूत्र होता है। ये आत्मा को बन्ध-त्रय में आबद्ध कर देते हैं। ये गुण न्याय तथा वैशेषिक में निरूपित गुणों से भिन्न हैं। ये प्रकृति के वास्तविक उपादान तत्व हैं। ये प्रकृति से आविर्भूत समस्त विश्व को रूपायित करते हैं। ये परस्पर सम-रूप न हो कर विषम-रूप होते हैं। इनमें से किसी एक या अन्य का आधिक्य हता है। जिस प्रकार वेदान्त में सत्-चित्-आनन्द की त्रिपुटी है, उसी प्रकार सांख्य में कुणे की त्रिपुटी है।
गुणों के अन्तर्व्यापार से विकास
तीनों गुण कभी एक-दूसरे से पृथक् नहीं होते। ये एक-दूसरे के सहायक तथा परस्पर मिश्रित होते हैं। ज्योति, तैल तथा दीप-शिखा में जो सम्बन्ध होता है, वहीं अन्तरंग सम्बन्ध इन गुणों में भी होता है। ये प्रकृति के सार-तत्त्व हैं। सभी वस्तुओं की सृष्टि इन तीन गुणों से ही होती है। इनकी एक-दूसरे पर प्रतिक्रिया होती रहती है। तभी अभिव्यक्ति या विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। नाश केवल तिरोभाव है।
गुण 'प्रमेय' तथा पुरुष 'साक्षी प्रमाता' है। पुरुष से प्रभावित हो कर ही प्रकृति विकास की क्रिया में संलग्न होती है। अखिल विश्व का कारण महत् अर्थात् बुद्धि प्रकृति के विकास की प्रथम विकृति है। बुद्धि के पश्चात् अहंकार का आविर्भाव होता है। कर्तृत्व अहंकार का धर्म है। इस तत्त्व से वैयक्तिक वैभिन्य का आविर्भाव होता है। अहंकार से मन उत्पन्न होता है जो कर्मेन्द्रियों के माध्यम से इच्छाओं का आज्ञा-पालन करता है। यह संकल्प-विकल्प करता है। यह इन्द्रियों के व्यापार को ज्ञान या बोध में संश्लेषित करता है। यह इन्द्रिय-प्रत्यक्ष तथा कर्म-दोनों में भाग लेता है। सांख्य की पद्धति में प्राण-तत्त्व का कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है, जब कि वेदान्त में यह एक पृथक् तत्त्व है। सांख्य की पद्धति के अनुसार मन द्वारा इन्द्रियों से पंच प्राणों की उत्पत्ति होती है। प्राण इन्द्रियों का रूपान्तरण है। इनके अभाव में इसकी सत्ता नहीं रहती।
तीनों गुणों के लक्षण
सत्त्व समत्व तथा सन्तुलन है। प्रबलता की अवस्था में यह शान्तिदायक होता है। रजस् में क्रियाशीलता होती है। यह स्वयं को राग-द्वेष, प्रेम-घृणा तथा आकर्षण-विकर्षण के रूप में अभिव्यक्त करता है। तमस् अकर्मण्यता, जड़ता तथा विकर्म की ओर अभिमुख रहता है। इससे मोह तथा अविवेक उत्पन्न होते हैं।
जब सत्त्व की प्रधानता होती है, तब यह रजस् तथा तमस् को कुण्ठित कर देता है। इसी प्रकार जब रजस् की प्रधानता होती है, तब यह सत्त्व तथा तमस् को कुण्ठित कर देता है और तमस् अपनी प्रधानता की अवधि में रजस् तथा सत्त्व को प्रभावशून्य कर देता है।
तीन गुणों का मनुष्य पर प्रभाव
ये तीन गुण प्रत्येक मनुष्य में हैं। कभी-कभी उसमें सत्त्व-गुण की प्रधानता हो जाती है। इस स्थिति में वह शान्त-चित्त हो कर चिन्तन तथा ध्यान करता है। किन्तु जब उसकी प्रकृति रजस्-प्रधान होती है, तब वह विभिन्न जागतिक कर्मों में लिप्त हो कर वासना और क्रियाशीलता से उद्वेलित हो उठता है। तमस् की प्रधानता में वह आलसी, मन्दबुद्धि तथा निष्क्रिय हो जाता है। तमस् से भ्रम उत्पन्न होता है।
विभिन्न व्यक्तियों में सामान्यत: इन तीनों में से किसी एक गुण की प्रधानता होती है। सात्त्विक मनुष्य सदाचारी होता है। वह पवित्र एवं निष्कल्मष जीवन व्यतीत करता है। राजसिक मनुष्य में आवेग तथा सक्रियता की प्रधानता होती है और तामसिक मनुष्य मन्दबुद्धि तथा निष्क्रिय होता है।
सत्त्व मनुष्य को दिव्य तथा उदात्त, रजस् सांसारिक तथा स्वार्थी और तमसू पशुवत् तथा अज्ञानी बनाता है। साधु-सन्तों में सत्त्च तथा सैनिकों, राजनयिकों और व्यापारियों में रजस् अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है।
पुरुष
पुरुष के लक्षण
पुरुष प्रकृति से परे है। यह उससे नित्य भिन्न या मूलतः पृथक् है। पुरुष अनादि, अनन्त, निर्गुण तथा निर्विशेष है। यह सूक्ष्म, सर्वव्यापी एवं मन, बुद्धि, इन्द्रिय, काल, दिक् तथा कार्य-कारण-सम्बन्ध के परे है। यह नित्य द्रष्टा, पूर्ण, अविकार्य तथा चिद्रूप है ।
पुरुष कर्ता न हो कर साक्षी है। यह स्फटिक-मणि की भाँति वर्णहीन है। यह अपने सम्मुख प्रस्तुत किये गये विभिन्न वर्णों के कारण ही रंजित प्रतीत होता है। यह भौतिक नहीं है। निरवयव होने के कारण यह अनश्वर है। सांख्य के अनुसार पुरुष या आत्माएँ असंख्य हैं। यदि पुरुषों की संख्या एक होती, तो एक की मुक्ति से सभी मुक्त हो जाते।
मूलतः विभिन्न पुरुषों में स्वभावगत समरूपता है। गतिहीनता पुरुष की नियति है। मुक्त होने के पश्चात् उसका कोई गन्तव्य नहीं रह जाता।
पुरुषों में जो परस्पर पार्थक्य है, वह नित्य है। प्रकृति के साथ इनके सम्बन्ध में भी इसी पार्थक्य के दर्शन होते हैं। प्रत्येक पुरुष में एक अपनी वैयक्तिकता होती है जो सभी देहान्तरणों में अपरिवर्तनीय बनी रहती है। प्रत्येक पुरुष एक पृथक् सृष्टि का साक्षी होता है और इसके प्रति तटस्थ रहता है। वह अन्ध-पंगुन्यायानुसार प्रकृति से संयुक्त हो कर सृष्टि के व्यापार का अवलोकन किया करता है जिसमें प्रकृति स्वयं असमर्थ है।
पुरुष अथवा आत्मा साक्षी, द्रष्टा, मध्यस्थ कैवल्य, अकर्ता तथा उदासीन है।
पुरुष की सत्ता का अनुमान
चेतना बुद्धि का धर्म नहीं हो सकती; क्योंकि बुद्धि भौतिक तथा प्रकृति का परिणाम है जो स्वयं अचेतन है। यदि कारण में चेतना का अभाव है, तो वह कार्य में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाने में असमर्थ है। अतः चेतना का एक सुस्पष्ट तत्त्व होना ही चाहिए और वह तत्त्व है पुरुष या आत्मा।
आत्मा की सन्निधि के कारण जड़ शरीर चेतन तथा आत्मा कर्ता प्रतीत होता है। जिस प्रकार शीतल जल से पूर्ण घट शीतल तथा उष्ण जल से पूर्ण घट उष्ण प्रतीत होता है, उसी प्रकार मन आदि भी पुरुष के संयोग से चेतन प्रतीत होने लगते हैं। धर्मो का यह पारस्परिक स्थानान्तरण अग्नि तथा अयस या सूर्य तथा जल की भाँति है।
प्रकृति के व्यापार के पर्यवेक्षण के लिए प्रकृति की अपेक्षा किसी उच्चतर तत्त्व की आवश्यकता है। यह पर्यवेक्षक उच्चतर तत्त्व पुरुष या आत्मा ही है। प्रकृति तथा इसकी विकृति भोग के विषय हैं। इनके भोग के लिए किसी ऐसे भोक्ता का होना अनिवार्य है जो चेतन हो। यह चेतन भोक्ता पुरुष या आत्मा ही है।
जिस प्रकार कुरसी तथा मेज की उपयोगिता किसी अन्य के लिए है उसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय तथा मन की उपयोगिता आत्मा के लिए है, जो गुणों से असम्पृक्त अथवा निर्गुण होने के कारण अभौतिक है। पुरुष गुणों का साक्षी तथा गुण विषय अथवा प्रमेय हैं। पुरुष साक्षी प्रमाता है। अतः वह सुख, दुःख तथा मोह, जो क्रमशः सत्त्व, रजस् तथा तमस् के धर्म हैं, से क्षुब्ध नहीं होता। यदि दुःख पुरुष का स्वाभाविक धर्म है और यदि वह गुणत्रय के व्यापार से स्वभावतः मुक्त नहीं है, तो पुनर्जन्म से उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है।
पुरुष तथा प्रकृति : एक विरोधाभास
पुरुष तथा प्रकृति के लक्षण एक-दूसरे से स्वभावतः भिन्न हैं। पुरुष चेतन, निष्क्रिय, निर्गुण तथा अविकार्य है, जब कि प्रकृति जड़, सक्रिय, त्रिगुणात्मक तथा परिणामी है।
विश्व
जब प्रकृति की साम्यावस्था में क्षोभ उत्पन्न होता है, तब अपने विभिन्न तत्वों से युक्त इस विश्व का आविर्भाव होता है। प्रकृति पर असंख्य पुरुषों की एक यान्त्रिक प्रक्रिया होती है जिससे प्रकृति की साम्यावस्था में क्षोभ उत्पन्न होता है और उससे उसमें गतिशीलता आ जाती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।
विकास तथा प्रत्यावर्तन
प्रकृति संसार का मूल है। यह प्रकृति ही संसार का निमित्त तथा उपादान, दोनों कारण है। प्रकृति से समष्टिगत बुद्धि अर्थात् महत् तथा महत् से समष्टिगत अहंकार उत्पन्न होता है। आत्मगत पक्ष में समष्टिगत अहंकार से मन-सहित एकादश इन्द्रियाँ तथा वस्तुगत पक्ष में शब्द, गन्ध, रस, रूप तथा स्पर्श-ये तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। इन पंचतन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तैजस्, वायु तथा आकाश पंच स्थूल भूतों का आविर्भाव होता है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध क्रमशः आकाश, वायु, तैजस्, अपस् तथा पृथ्वी के गुण हैं जो क्रमशः कर्णेन्द्रिय, त्वचा, नेत्रेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय तथा घ्राणेन्द्रिय के विषय हैं। प्रथम भूत के अतिरिक्त अन्य सभी भूतों में अपने गुणों के अतिरिक्त अपने पूर्ववर्ती भूतों के गुण भी विद्यमान रहते हैं।
प्रलयकाल में प्रकृति की विकृतियों का प्रत्यावर्तन विकास के पूर्ववर्ती चरणों में विपरीत गति से होता है और अन्ततः इसका अन्तर्लयन प्रकृति में हो जाता है। पृथ्वी अपने कारण जल में, जल तैजस् में, तैजस् वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महत् में तथा महत् प्रकृति में विलीन हो जाता है। अन्तर्लयन की प्रक्रिया यही है। संसार या प्रकृति की लीला अनन्त है। विकास तथा अन्तर्लयन के इस चक्र का न आदि है, न अन्त।
ज्ञान की प्रक्रिया
इन्द्रियाँ विषय से उद्दीप्त होती हैं और मन इन्द्रिय-विषय-सन्निकर्ष-जनित संवेदनों को निर्विकल्प ज्ञान में व्यवस्थित कर देता है। इसके पश्चात् अहंकार इसे आत्मा को सम्प्रेषित करता है और बुद्धि इस निर्विकल्प ज्ञान को एक अवधारणा अथवा सविकल्प ज्ञान में रूपान्तरित कर पुरुष के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। इस प्रकार वस्तु का ज्ञान होता है।
किसी विषय से सम्बन्धित होने के पूर्व सर्वप्रथम आप उसका अवलोकन तथा उस पर विचार करते हैं। इसके पश्चात् उस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके पश्चात् आप कर्तृत्व के अभियान में अग्रसर होते हैं। यह निश्चय कि यह कार्य मुझसे ही सम्पन्न होना चाहिए, बुद्धि का संकल्प (अध्यवसाय) है। बुद्धि एक माध्यम या करण है जो मन तथा इन्द्रिय द्वारा सम्प्रेषित संवेदनों को ग्रहण करें इन्हें एक सुनिश्चित प्रत्यय में रूपान्तरित करती और तत्पश्चात् इन्हें आत्मा के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। निश्चय बुद्धि का व्यापार है।
मन संवेदन तथा क्रिया, दोनों का करण है। इन्द्रियाँ सामान्य संवेदनों को ग्रहण करती हैं और मन तथा इन्द्रियों के परस्पर सहयोग से इन संवेदनों का प्रत्यक्षीकरण होने लगता है। मन मननशील, बुद्धि निश्चयात्मिका तथा अहंकार चेतन हो जाता है।
कर्तृत्व अहंकार में होता है। अहंकार अहंभावना का स्रष्टा है जो स्वयं प्रकृति की एक विकृति है; किन्तु इसका पुरुष से कोई सम्बन्ध नहीं होता जो सदैव एक साक्षी के रूप में अवस्थित रहता है।
बुद्धि, अहंकार, मन तथा नेत्र एक ही साथ किसी वस्तु के आकार को देख कर तत्क्षण कह उठते हैं- "यह घट है।" इन तीनों को किसी विषय के रस, गन्ध, शब्द तथा स्पर्श का ज्ञान क्रमशः रसना, घ्राण, कर्ण तथा त्वक् इन्द्रियों से होता है। कभी-कभी यह प्रक्रिया आनुक्रमिक रूप से भी होती है। किसी मार्ग पर चलते हुए कोई मनुष्य किसी दूरस्थ वस्तु को देखता है, तो उसके मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि यह कोई स्तम्भ है या मनुष्य; किन्तु जब वह उस वस्तु पर किसी पक्षी को बैठे हुए देखता है तब विचार या मनन के द्वारा उसकी शंका की निवृत्ति हो जाती है और बुद्धि इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच जाती है कि यह एक स्तम्भ है। इसके पश्चात् अहंकार कह उठता है- "मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह एक स्तम्भ मात्र है।" इस प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार तथा नेत्र के व्यापार आनुक्रमिक रूप से होते हैं। नेत्रों के पास देखने के लिए, मन के पास विचार या मनन के लिए, अहंकार के पास क्रियान्वयन के लिए तथा बुद्धि के पास निश्चय के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है। एक अन्य दृष्टान्त से इसे स्पष्ट किया जा रहा है। कान धनुष की प्रत्यंचा का गम्भीर घोष सुनते हैं और मन विचार करता है कि यह बाण के प्रक्षेपण का संकेत है। अहंकार कहता है- “इसका लक्ष्य मैं ही हूँ" और बुद्धि कहती है-"अब मुझे यहाँ से शीघ्र ही अन्यत्र चले जाना चाहिए।"
बुद्धि, मन तथा अहंकार द्वारपाल हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ द्वार हैं और बुद्धि वह माध्यम है जो इन्द्रियों और आत्मा के बीच मध्यस्थ है।
बुद्धि तथा इसका व्यापार
प्रकृति की समस्त विकृतियों में बुद्धि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकृति है। इन्द्रियाँ अपने विषयों को इसी के समक्ष प्रस्तुत करती हैं और तत्पश्चात् बुद्धि उसे पुरुष को प्रेषित करती है। यह पुरुष तथा प्रकृति के पारस्परिक भेद को भी विवेचित करती है।
बुद्धि आत्मा तथा इन्द्रियों के बीच सम्बन्ध-स्थापन का एक माध्यम है। संवेदन, मनन तथा चेतना से अधिगत प्रत्ययों से आत्मा के अवगत होने से पूर्व ही उक्त प्रत्यय मुख्य तथा महान् कारण बुद्धि में संग्रहीत हो जाते हैं। वस्तुतः इनका संग्रहण आत्मा के उपभोग के लिए ही होता है। ये सत्त्व, रजस् तथा तमस् के गुणों के आनुपातिक प्रभाव के अनुसार सुख, दुःख तथा उदासीनता से प्रभावित प्रत्ययों को प्रस्तुत करते रहते हैं।
जिस प्रकार एक ग्रामप्रधान ग्रामवासियों से कर-संग्रह कर जिलाधिकारी को सौंपता है, जिस प्रकार स्थानीय जिलाधिकारी इस धन-राशि को मंत्री को सौंप देता है और जिस प्रकार मन्त्री इस धन का ग्रहण राज्य के उपयोग के लिए करता है उसी उकार मन इन प्रत्ययों को बाह्येन्द्रियों से प्राप्त कर अहंकार को और अहंकार इन्हें बुद्धि को सौंप देता है जो मुख्य अधीक्षक है और जो इन प्रत्ययों का उपयोग सर्वप्रभुतासम्पन्न आत्मा के लिए करती है।
बुद्धि आत्मा का महामात्य है। वह पुरुषों के समक्ष भोग्य कर्म-फलों को प्रस्तुत किया करती है। वह अपने अत्यन्त निकटस्थ पुरुष से प्रतिबिम्बित होने के कारण चेतन प्रतीत होती है; किन्तु स्वयं वह अचेतन है।
जीव
जीव इन्द्रियों से संयुक्त आत्मा है। यह शरीर द्वारा परिच्छिन्न है। इसमें अहंकार है। बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब अहंकार या अनुभवकर्ता आत्मा की भाँति प्रतीत होता है। यह अज्ञान तथा कर्म से सम्बद्ध होने के अतिरिक्त सुख, दुःख तथा इसके फलों के अधीन एवं जन्म-मरण के चक्र में आबद्ध है।
जीव के लिए पुरुष की पूर्णता एवं उसकी स्थिति तथा महिमा की सम्प्राप्ति अनिवार्य है। प्रत्येक जीव में उच्चतर पुरुष परोक्ष रूप से विद्यमान है। उसके लिए इस उच्चतर पुरुष के यथार्थ स्वरूप से परिचित होना नितान्त आवश्यक है। स्वतन्त्रता अथवा पूर्णत्व अपने वास्तविक स्वरूप की ओर प्रत्यावर्तन तथा उसके इस यथार्थ स्वरूप को आवृत करने वाले अध्यास की निवृत्ति है।
मुक्ति
बन्ध का सम्बन्ध प्रकृति से है; किन्तु इसका अध्यारोप पुरुष पर किया जाता है। वस्तुतः पुरुष नित्य-मुक्त है। अविवेक के कारण पुरुष तथा प्रकृति में एकत्व-दर्शन संसार अथवा बन्ध का कारण है और विवेक द्वारा पुरुष तथा प्रकृति में भेद-दर्शन मुक्ति है। मुक्ति निरपेक्ष सत्ता में अन्तर्लयन न हो कर प्रकृति से पार्थक्य है।
प्रकृति से संयुक्त होने के कारण पुरुष या आत्मा अविद्या के बन्धन में आबद्ध हो जाता है। सांख्य-दर्शन का प्रयोजन पुरुष को इससे मुक्त करना है। सृष्टि के अंगांगिभूत चौबीस तत्त्वों तथा आत्मा से इनके पार्थक्य के निर्धान्त ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है।
संसार में विद्यमान वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांख्य-दर्शन तीन प्रमाणों को स्वीकृत करता है। ये प्रमाण हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्त वचन।
मुक्ति की प्रक्रिया
जब पुण्य-पाप आदि के परिणामों के फलस्वरूप आत्मा का शरीर से सम्बन्ध-विच्छेद होता है और जब प्रकृति उसके सम्बन्ध में नितान्त निष्क्रिय हो जाती है, तब अन्तिम तथा निरपेक्ष मुक्ति एवं आत्यन्तिक दिव्य प्रकाश-युक्त सौन्दर्य का सूर्योदय होता है।
जब कर्मों के परिणाम उपरामावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों का विघटन हो जाता है, तब जीव के लिए प्रकृति अस्तित्वहीन हो जाती है। जीव कैवल्यावस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था में वह त्रिविध ताप से मुक्त हो जाता है।
बुद्धि, अहंकार, मन, पंचज्ञानेन्द्रियाँ, पंचकर्मेन्द्रियाँ तथा पंचतन्मात्राएँ लिंगदेह अथवा सूक्ष्म शरीर के संघटक तत्त्व हैं। यह सूक्ष्म शरीर आनुक्रमिक जन्मों में एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में रूपान्तरित होता रहता है। विभिन्न जन्मों के कर्मों के संस्कार सूक्ष्म शरीर में संचित होते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर का संयोग जन्म तथा इनका पार्थक्य मृत्यु है। पुरुष के ज्ञान से इस सूक्ष्म शरीर या लिंगदेह की निवृत्ति हो जाती है।
जब किसी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब पुण्य-पाप कारण-अविद्या-शक्ति से रहित हो जाते हैं। किन्तु जिस प्रकार कुम्भकार द्वारा चक्र-परिचालन की क्रिया के स्थगन के बाद भी चक्र कुछ क्षणों तक गतिशील रहता है, उसी प्रकार प्रारब्ध के कारण मुक्त पुरुष का शरीर भी कुछ समय के लिए विद्यमान रह जाता है।
मुक्ति ही प्रकृति के व्यापार का समापन है
पुरुष-प्रकृति-संयोग अन्तर-पारा, अपार होता है। एक बार दो व्यक्ति, जिनमें एक नेत्रहीन था तथा दूसरा पंगु, अपने सहयात्रियों से विलग हो गये। इनमें से एक ने मार्ग-दर्शन तथा दूसरे से संचरण का उत्तरदायित्व वहन कियो गये। नेत्रहीन का पथ-प्रदर्शन करता तथा नेत्रहीन उसके संकेतानुसार आगे बढ़ता। आत्मा उक्त पंगु की भाँति है। उसमें दर्शन-शक्ति है; किन्तु उसमें गतिशीलता का अभाव है उसके विपरीत प्रकृति में गतिशीलता तो है; किन्तु वह दर्शन-शक्ति से रहित है। वह दुसरा नेत्रहीन व्यक्ति की भाँति है। जब उक्त नेत्रहीन तथा पंगु व्यक्ति अपने गन्तव्य तक पहुँच गये, तब वे एक-दूसरे से अलग हो गये। इसी प्रकार प्रकृति पुरुष की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर उपरामावस्था को प्राप्त हो जाती है और पुरुष को कैवल्य अथवा शाहयक्तिक दिव्य सौन्दर्य की प्राप्ति हो जाती है। इसके फलस्वरूप पुरुष तथा प्रकृति के निर्धारित प्रयोजनों की सिद्धि हो जाती है और तत्पश्चात् इनके पारस्परिक सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार पुरुष प्रकृति के ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है।
प्रकृति का व्यापार पुरुष के लाभार्थ तथा भोगार्थ होता है। प्रकृति पुरुष का हाथ एकड़ कर उसे जागतिक प्रपंच-दर्शन तथा उसके भोग में प्रवृत्त करते हुए अन्ततः उसे मुक्ति-प्राप्ति में सहयोग प्रदान करती है।
वस्तुतः आत्मा न बद्ध है न मुक्त। उसका देहान्तरण भी नहीं होता। यह प्रकृति हो है जो अनेक पुरुषों के सन्दर्भ में बद्ध, मुक्त तथा देहान्तरित होती रहती है।
जिस प्रकार कोई नृत्यांगना दर्शकों के समक्ष मंच पर अपने नृत्य का प्रदर्शन कर उसका समापन कर देती है, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष स्वयं को अनावृत या व्यक्त करने के पश्चात् अपने व्यापार से निवृत्त हो जाती है। जब वह इस तथ्य से परिचित हो जाती है कि पुरुष उसकी लीला से पूर्णतः परिचित हो चुका है, तब वह नितान्त संकुचित तथा शालीन हो जाती है और पुरुष के समक्ष पुनः आत्म-प्रदर्शन नहीं करती।
योग
भूमिका
दर्शन की राजयोग-पद्धति के प्रतिपादक, योग के प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित आप प्रदान करने वाले तथा योग की आदि पाठ्य-पुस्तक 'योगसूत्र' के प्रणेता श्री सर्वांत महर्षि को प्रणाम !
योग शब्द की निष्पत्ति युज् धातु से हुई है जिसका अर्थ है जोड़ना। योग चित्तवृत्ति-निरोध तथा वैयक्तिक आत्मा का सर्वोच्च आत्मा से सम्प्रयोग है। हिरण्यगर्भ योग-पद्धति के प्रवर्तक हैं। पतंजलि महर्षि द्वारा प्रवर्तित योग सांख्य की एक शाखा अथवा अनुपूरक है। रहस्यवादी तथा मननशील विद्यार्थियों के लिए इसका एक विशिष्ट सम्मोहन है। सर्वोच्च सत्ता अर्थात् ईश्वर के अस्तित्व के प्रति अपनी स्पष्ट आस्था के कारण यह दर्शन शास्त्रसम्मतता तथा पुरातनता के सम्बन्ध में अपना पक्ष मुख्य सांख्य की अपेक्षा प्रबलतर रूप में प्रस्तुत करता है।
पतंजलि का ईश्वर क्लेश-कर्म-विपाक-आशय-रहित पुरुष-विशेष है। वह निरतिशय सर्वज्ञता का बीज-स्वरूप है। काल से अनवच्छिन्न होने के कारण वह पुरातन गुरुओं का भी गुरु है।
पवित्र अक्षर ॐ ईश्वर का अभिधायक या वाचक है। ॐ शब्द की आवृत्ति तथा उसकी भावना या उसके ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे विघ्न-बाधाओं की निवृत्ति तथा ईश्वर-साक्षाकार होता है।
योगसूत्र
पतंजलि का योगसूत्र योग का सर्वाधिक पुरातन ग्रन्थ है। यह चार अध्यायों में विभक्त है। इसके प्रथम अध्याय 'समाधिपाद' में समाधि के स्वरूप तथा उद्देश्य का वर्णन है तथा द्वितीय अध्याय 'साधनपाद' में इसके उद्देश्य की प्राप्ति के साधनों की व्याख्या की गयी है। तृतीय अध्याय 'विभूतिपाद' में योगाभ्यास से प्राप्त अलौकिक शक्तियों अथवा सिद्धियों का तथा चतुर्थ अध्याय 'कैवल्यपाद' में मुक्ति के स्वरूप का वर्णन किया गया है।
राजयोग तथा हठयोग
पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग को अष्टांगयोग कहते हैं। यह अष्टावयवी है। अष्टांगयोग का सम्बन्ध मन के अनुशासन तथा अतीन्द्रिय शक्तियों से है, जब कि हठयोग का सम्बन्ध शारीरिक नियन्त्रण तथा श्वास-प्रश्वास के नियमन की विधियों से है। हठयोग की परिसमाप्ति राजयोग में होती है। हठयोग की पुरोगामी साधना साधक को राजयोग की निष्पत्ति की दिशा में अग्रसर होने के लिए उत्प्रेरित करती है। हठयोग राजयोग के विभिन्न चरणों या उसके उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए एक सोपान है। जब कुम्भक के द्वारा श्वास की गति अवरुद्ध हो जाती है, तब मन निराश्रित हो जाता है। शरीर-शुद्धि तथा श्वास का नियन्त्रण हठयोग के अव्यवहित उद्देश्य हैं। षट्कर्म अर्थात् शरीर-शुद्धि की क्रियाएँ निम्नांकित हैं।
१. धौति अर्थात् आमाशय-शुद्धि।
२. वस्ति अर्थात् एनिमा का प्राकृतिक रूप।
३. नेति अर्थात् नासारन्ध्रों की शुद्धि।
४. त्राटक अर्थात् किसी वस्तु पर निर्निमेष दृष्टिपात।
५. नौलि अर्थात् उदर को चक्राकार घुमाना।
६. कपालभाति अर्थात् प्राणायाम की एक निश्चित विधि से श्लेष्मा का निराकरण।
आसन, बन्ध तथा मुद्रा के अभ्यास से शरीर स्वस्थ, सुदृढ़ तथा सन्तुलित रहता है।
योग : मनोनिग्रह का एक सुव्यवस्थित प्रयास
योग कठोर अनुशासन की एक पद्धति है। इसमें आहार, निद्रा, संगति, आचरण, वाणी तथा विचार के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्धों की व्यवस्था है। योगाभ्यास किसी कुशल तथा प्रबुद्ध योगी के निर्देशन में करना चाहिए।
योग मन के नियन्त्रण तथा पूर्णत्व के अधिगम का एक सुव्यवस्थित प्रयास है। यह धारणा-शक्ति को समृद्ध करता है, मन के इतस्ततः अर्थहीन विचरण को प्रतिबन्धित करता है और लोकोत्तर चेतना अर्थात् निर्विकल्प समाधि की सम्प्राप्ति में योगदान देता है। योगाभ्यास से मन तथा शरीर की उद्विग्नता का निराकरण होता है। यह मानसिक विकारों को विनष्ट कर मन को दृढ़ता प्रदान करता है। योग का उद्देश्य जीव को उन साधनों की सम्प्राप्ति की कला में प्रशिक्षित करना है जिनसे वह परमात्मा के पूर्ण सायुज्य को प्राप्त होता है। चित्त-वृत्तियों के निरोध से ही परमात्मा से यह सायुज्य निष्पन्न हो पाता है। यह स्थिति स्फटिक-मणि की भाँति निर्मल होती है; क्योंकि इसमें जागतिक पदार्थों के सम्पर्क के कारण मन कलुषित नहीं रहता।
योग तथा सांख्य
कपिल की पद्धति में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, अतः इसे निरीश्वर सांख्य कहते हैं; किन्तु पतंजलि की पद्धति सेश्वर सांख्य है। वह उस पुरुष-विशेष के भति आस्थावान् है जो क्लेश, कर्म तथा वासनादि से अपरामृष्ट है। पतंजलि ने अपनी
पद्धति की संरचना सांख्य की तत्त्वमीमांसा की पृष्ठभूमि पर की। वे सांख्य के पचीस तत्त्वों को स्वीकृत करते हुए इसके तत्वशास्त्रीय दृष्टिकोण के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हैं; किन्तु वे पुरुष-विशेष अथवा ईश्वर के साथ निरपेक्ष एकत्व के साक्षात्कार के लिए आत्मानुशासन के व्यवहार-पक्ष पर अधिक बल देते हैं।
सांख्य तत्त्वमीमांसा की और योग व्यावहारिक अनुशासन की पद्धति है। इन दोनों में पूर्व पक्ष अनुसन्धान तथा तर्क को और उत्तर पक्ष इच्छा-शक्ति की धारणा को अधिक महत्त्व प्रदान करता है।
योग में जीव को अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। उसे ईश्वर की कृपा से मुक्ति-लाभ हो सकता है। सांख्य के अनुसार मुक्ति का साधन ज्ञान है, जब कि योग के अनुसार धारणा, ध्यान तथा समाधि से मुक्ति प्राप्त होती है। योग की मान्यता है कि चित्त की वृत्तियों की असादृश्यता का निरोध तथा स्वयंप्रकाश पुरुष पर मन की धारणा या एकाग्रता में ही योग की प्रक्रिया निहित है।
राजयोग के अष्टावयव
राजयोग को अष्टांगयोग के नाम से जाना जाता है। ये अष्टावयव यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि हैं। इनमें से प्रथम पाँच बहिरंगयोग के अन्तर्गत तथा शेष तीन अन्तरंगयोग के अन्तर्गत आते हैं।
यम और नियम
नैतिक अनुशासन यम तथा नियम के अभ्यास में निहित है। ये योग के विद्यार्थियों के लिए योग के वास्तविक अभ्यास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। योग के विद्यार्थी को यम के पंचांगों-अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह-का अभ्यास करना चाहिए। परिग्रह विलासिता की ओर उन्मुख करता है। योग के विद्यार्थी के लिए नियम के पंचांगों-शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान-का अभ्यास भी आवश्यक है। इनमें अहिंसा का प्रमुख स्थान है। समस्त प्राणियों के प्रति विद्वेष का सर्वथा तथा सर्वदा परित्याग अहिंसा है। इसमें अहिंसा के साथ-साथ अद्वेष भी निहित है। यम को महाव्रत कहा जाता है जो जाति, दिक् तथा काल से अप्रतिबन्धित है। इनका अभ्यास सबको करना चाहिए। इन सिद्धान्तों के लिए कोई अपवाद नहीं है। अहिंसा-व्रत के अभ्यासी के सम्बन्ध में आत्मरक्षा का तर्क भी हत्या के औचित्य की सिद्धि नहीं कर सकता। यदि उसे योग की अध्यास कठोरतापूर्वक करना है, तो उसे अपने शत्रु की भी हत्या नहीं करनी बाहिए।
आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार
स्थिर तथा सुखप्रद मुद्रा को आसन कहते हैं। इससे धारणा में शारीरिक रूप से भोगदान प्रास होता है। आसन में निष्णात व्यक्ति द्वन्द्वात्मक क्षोभ से मुक्त हो जाता है और प्राणायाम से मन की शान्ति तथा स्थिरता एवं सुस्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अन्तर्मुखता प्रत्याहार का स्वरूप है। यह इन्द्रियों का उनके विषयों से प्रत्यावर्तन है। धर्म, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार योग के सहायक उपांग हैं।
धारणा, ध्यान तथा समाधि
धारणा, ध्यान तथा समाधि मानसिक एकाग्रता की उसी प्रक्रिया की तीन अधिक स्थितियाँ हैं। इस प्रकार ये एक ही अंग के तीन संघटक तत्त्व हैं। किसी विषय पर मन की सुदृढ़ स्थिरता का प्रयास धारणा और किसी विषय पर मन की अविच्छिन्न हाथा अप्रतिहत एकाग्रता ध्यान है। समाधि वह अवस्था है जिसमें मन किसी विषय पर इन आत्यन्तिक तन्मयता के साथ एकाग्र या स्थिर हो जाता है कि वह स्वयं बेय-वस्तु के रूप में परिणत हो जाता है। इस स्थिति में मन जिस विषय पर स्थिर हुआ रहता है, उसमें वह पूर्णतः विलीन हो कर उसके तद्रूप हो जाता है।
संयम अथवा धारणा, ध्यान तथा समाधि एक तथा समरूप हैं जिनसे अतीन्द्रिय विषयों का बोध होता है। सिद्धियाँ संयम का उपफल हैं। लोकोत्तर शक्तियाँ समाधि या मुक्ति के मार्ग में वस्तुतः अवरोध उपस्थित करती हैं।
योग-समाधि तथा इसका स्वरूप
ध्यान का उद्देश्य समाधि है और समाधि ध्यान की अधिमात्रता है। यह योगानुशासन का लक्ष्य है। इस अवस्था में मन तथा शरीर बाह्य प्रभावों के लिए अस्तित्वशून्य हो जाते हैं तथा बाह्य जगत् से इनका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। समाधि में योगी एक ऐसे दिव्य तथा निःशब्द लोक में प्रविष्ट हो जाता है जो बाह्य ससार के अनवरत कोलाहल से सर्वथा असम्पृक्त है। इन्द्रियों का अन्तर्लयन मन में हो जाता है और मन अपने व्यापार से विरत हो जाता है। जब मन की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब द्रष्टा अथवा पुरुष आत्मस्थ हो जाता है। पतंजलि अपने योगसूत्र में इस स्थिति का उल्लेख 'स्वरूपेऽवस्थानम्' के रूप में करते हैं।
सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात-मात्रा-भेद से समाधि के ये दो रूप हैं। सम्प्रज्ञात-समाधि में ध्यान की स्थिरता के लिए एक निश्चित विषय होता है और मन इस विषय से अभिज्ञ रहता है। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानन्द तथा सस्मिता सम्प्रज्ञात-समाधि के रूप हैं। सम्प्रज्ञात-समाधि में ध्याता को ध्येय-विषय का स्पष्ट ज्ञान बना रहता है; किन्तु असम्प्रज्ञात-समाधि में पृथकता के इस ज्ञान का अतिक्रमण हो जाता है जिसके फलस्वरूप यह लुप्त हो जाता है।
राजयोग में सफलता के लिए अपेक्षित माध्यम यम तथा नियम का महत्त्व
ईश्वर-साक्षात्कार के आकांक्षी को योग के समस्त अष्टावयवों का अभ्यास करना चाहिए। अष्टांगयोग के अभ्यास द्वारा काषाय के निराकरण के पश्चात् दिव्य ज्ञान के उस प्रकाश का आविर्भाव होता है जिससे भेदमूलक ज्ञान की सम्प्राप्ति होती है।
समाधि-लाभ के लिए यम-नियम का अभ्यास एक अनिवार्य आवश्यकता है। योग के विद्यार्थी को यम का अभ्यास तथा नियम का पालन साथ-साथ करना चाहिए। यम तथा नियम के अभाव में सम्यक् ध्यान की सम्प्राप्ति असम्भव है। मिथ्या, छल, निर्दयता तथा वासनादि की निवृत्ति के बिना आपके मन की एकाग्रता सम्भव नहीं है और मन की स्थिरता के अभाव में ध्यान तथा समाधि का प्रश्न ही नहीं उठता।
पतंजलि द्वारा प्रतिपादित पद्धति में चित्त की पंचभूमियाँ
पतंजलि की राजयोग-पद्धति के अनुसार क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध-मन की ये पाँच अवस्थाएँ हैं। क्षिप्तावस्था में मन विभिन्न इन्द्रिय विषयों में विचरण किया करता है। इसमें रजस् परिव्याप्त रहता है। तमस्-प्रधान मूढ़ावस्था में मन निद्रा तथा स्त्यान अथवा अकर्मण्यता की स्थिति में रहता है। विक्षिप्तावस्था में सत्त्व की प्रधानता होती है। इसमें मन ध्यान तथा विषयों के बीच अनिश्चितता की स्थिति में डोलता रहता है। इसमें चित्तवृत्तियों का शनैः-शनैः एकत्रीकरण होता है। जब सत्त्व में वृद्धि होती है, तब आपको मुदिता, इन्द्रिय-विजय तथा आत्म-साक्षात्कार के लिए अपेक्षित पात्रता की उपलब्धि होती है। एकाग्रावस्था में मन की एकाग्रता तथा ध्यान की गहनता की प्राप्ति होती है। इसमें सत्त्व रजस् तथा तमस् से मुक्त हो जाता है। निरुद्धावस्था मन के पूर्ण नियन्त्रण तथा वृत्तियों के निराकरण की अवस्था है।
वृत्ति मन के सरोवर में विचार-तरंगों का चक्रवात है। प्रत्येक वृत्ति अपने पीछे एक संस्कार छोड़ जाती है। अवसर प्राप्त होने पर यह संस्कार स्वयं को चेतनावस्था में अभिव्यक्त कर सकता है। वृत्तियाँ अपने अनुकूल प्रवृत्तियों को ही समृद्ध करती है। जब समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब मन 'समागति' अर्थात् सन्तुलित अवस्था में प्रविष्ट हो जाता है।
व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति-दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व अर्थात् समाधि में न पहुँचना और अनवस्थितत्व अर्थात् समाधि-भूमि की प्राप्ति पर भी उसमें चित्त का न ठहरना-ये चित्त के प्रमुख विक्षेप हैं।
पंचक्लेश तथा इनकी निवृत्ति
पतंजलि के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश पंचक्लेश हैं जो मन को क्षुब्ध किया करते हैं। निरन्तर योगाभ्यास से इनका उपशमन तो हो जाता है किन्तु इनका उच्च्छेद नहीं हो पाता। ये प्रच्छन्न रूप में बीज के रूप में विद्यमान रहते है। जब उन्हें अनुकूल अवसर तथा प्रतिवेश की प्राप्ति होती है, तब वे पुनः अंकुरित हो उठते हैं। किन्तु असम्प्रज्ञात-समाधि में इन अन्तरायों का पूर्ण उच्छेद हो जाता है और से निर्बीज हो जाते हैं।
अविद्या हमारे समस्त दुःखों का प्रधान कारण है। अहंकार अविद्या का हाक्कालिक परिणाम है। यह हमारे मन में राग-द्वेष की सृष्टि कर हमारी आध्यात्मिक तुहि को कुण्ठित कर देता है। योग-समाधि से अविद्या का नाश हो जाता है।
क्रियायोग का अभ्यास
क्रियायोग से मन की परिशुद्धि होती है। यह पंचक्लेशों को क्षीण कर मनुष्य को समाधि में प्रवृत्त करता है। तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान क्रियायोग के संघटक तत्त्व हैं।
समवयस्कों के प्रति मित्रता (मैत्री), कनिष्ठजनों के प्रति दया (करुणा), बौष्ठिजनों के प्रति प्रफुल्लता (मुदिता) तथा दुष्टजनों एवं सुख-दुःख तथा शुभ-अशुभ के प्रति उदासीनता (उपेक्षा) के अभ्यास से मानसिक शान्ति (चित्त-प्रसाद) की प्राप्ति होती है।
ईश्वर-भक्ति से समाधि-लाभ सम्भव है। इससे स्वातन्त्र्य अर्थात् मुक्ति की भी होती है। योग के विद्यार्थी को ईश्वर-प्रणिधान से भगवत्कृपा प्राप्त होती है।
अभ्यास तथा वैराग्य
मन के नियन्त्रण तथा उसकी स्थिरता में अभ्यास तथा वैराग्य सहायक होते हैं। जब भी कभी मन ऐन्द्रिय-विषयों की ओर आकर्षित हो, तब उसे पुनः-पुनः केन्द्र की ओर प्रत्याहारित करना चाहिए। यह अभ्यास योग है। इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ अनवरत रूप से निरन्तर करते रहने से यह स्थिर तथा सुदृढ़ हो जाता है। मन तृष्णाओं का भण्डार है। ये तृष्णाएँ वैराग्य के अभ्यास से नष्ट हो जाती हैं। वैराग्य मन को विषयों से विरत कर देता है। यह बहिर्मुखता को प्रतिबन्धित कर इसकी अन्तर्मुखता को सम्पुष्ट करता है।
कैवल्यावस्था अथवा निरपेक्ष स्वातन्त्र्य
प्रकृति से पुरुष की आत्यन्तिक अथवा निरपेक्ष पृथकता जीवन का लक्ष्य है। योग में मुक्ति को कैवल्य या निरपेक्ष स्वातन्त्र्य कहा गया है। इसमें आत्मा या पुरुष प्रकृति के बन्धनों से मुक्त हो कर अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जब आत्मा इस तथ्य से पूर्णतः परिचित हो जाता है कि अब उसे निरपेक्ष स्वतन्त्रता प्राप्त हो चुकी है और वह किसी भी जागतिक पदार्थ पर निर्भर नहीं है, तब वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। अब वह विवेक-ख्याति द्वारा अविद्या को नष्ट कर चुका होता है और पंचक्लेश ज्ञानाग्नि में विदग्ध हो चुके होते हैं। इस स्थिति में आत्मा चित्त के प्रतिबन्धों से अपरामृष्ट हो जाता है, गुण उपरामावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और आत्मा अपने दिव्य सारतत्त्व में स्थित हो जाता है; किन्तु उसकी मुक्ति के पश्चात् भी प्रकृति तथा उसके विकार अन्य लोगों के लिए विद्यमान रह जाते हैं। इस विषय में योग तथा सांख्य, दोनों का एक ही मत है।
पूर्वमीमांसा
भूमिका
श्री व्यास भगवान् के शिष्य तथा पूर्वमीमांसा-पद्धति के प्रवर्तक श्री जैमिनि को प्रणाम !
पूर्वमीमांसा अथवा कर्ममीमांसा वेदों के प्रारम्भिक भाग तथा इसकी यज्ञीय विधियों अथवा इसके मन्त्रों तथा ब्राह्मणों से सम्बन्धित प्रकरणों की अनुसन्धानात्मक परिपृच्छा है। इसे पूर्वमीमांसा इसलिए कहा जाता है कि यह उत्तरमीमांसा की अपेक्षा कालानुक्रमिकता के दृष्टिकोण से भले ही कुछ कम पूर्वकालीन हो, तार्किक अर्थ में अधिक पूर्वकालिक है।
मीमांसा : वेदों की व्याख्या की एक पद्धति
श्रीमांसा किसी दार्शनिक पद्धति की शाखा नहीं है। यह वैदिक निर्वचन की एक उति है। इसका दार्शनिक विवेचन ब्राह्मणों अथवा वेदों के आनुष्ठानिक प्रकरणों की आलोचनात्मक टिप्पणी की एक विधा मात्र है। यह वेदों की शाब्दिक व्याख्या करता है। पूर्वमीमांसा की केन्द्रिय समस्या कर्मकाण्ड या धार्मिक अनुष्ठान है। जैमिनि ने पूर्वमीमांसा के सूत्रों को व्यवस्थित कर अपनी कृति में इसकी प्रामाणिकता को सम्पुष्ट किया है। हिन्दू-विधि की व्याख्या के लिए इसके सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।
जैमिनि के मीमांसा-सूत्रों में विभिन्न यज्ञों, इनके प्रयोजनों तथा अपूर्व के सिद्धांत के अतिरिक्त कतिपय दार्शनिक स्थापनाओं का भी विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसमें बारह अध्याय हैं।
शबर जैमिनि के मीमांसा-सूत्र के प्रमुख भाष्यकार हैं। भवभूति के गुरु कुमारिल ने मुझे तथा भाष्य पर वार्त्तिक ग्रन्थों की रचना की। उन्होंने वेदों के नित्य-स्वरूप तथा वैदिक अनुष्ठानों की समीचीनता और क्षमता की सिद्धि की। प्रभाकर कुमारिल के विषय थे। उन्होंने शाबरभाष्य पर एक वार्त्तिक लिखा।
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द-जैमिनि इन तीन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार शब्द तथा इसके निहितार्थ में अविच्छिन्न सम्बन्ध है। वे शब्द को नित्य मानते हैं।
वेद : नित्य तथा अपौरुषेय
जैमिनि बुद्धिवाद तथा नास्तिकता के विरोधी थे। वस्तुतः उन्होंने वेद को ही ईश्वर माना था। नित्य वेद के आधार के लिए किसी अन्य अधिष्ठान की आवश्यकता ही है। इसका कोई दैवी उद्घाटक नहीं है। वेद स्वतःप्रमाण है। यह हमारे धर्म-ज्ञान या एकमात्र स्रोत है। ईश्वर उनके और उनकी पद्धति के लिए आवश्यक नहीं था। उनके अनुसार वेद स्वतःप्रमाण है। उन्होंने अपने प्रथम सूत्र में ही धर्म को अत्यन्त भावपूर्ण बताते हुए लिखा है : "अथातो धर्म-जिज्ञासा ।" इस सूत्र से उनके कोण उद्देश्य तथा प्रयोजन स्पष्ट हो जाते हैं। इस सूत्र के अनुसार यह उद्देश्य या हम उस धर्म या करणीय कर्म की जिज्ञासा है जिससे वेद-विहित अनुष्ठानों का
निष्पादन एवं यज्ञ समाविष्ट हैं। धर्म स्वयं पुरस्कार या सुफल प्रदान करता है। पूर्वमीमांसा का उद्देश्य धर्म के स्वरूप का अनुसन्धान है।
पूर्वमीमांसा अनेक देवताओं के प्रति आस्थावान् है। उन्हें हवि अर्पित की जा सकती है। वैदिक धर्म के पालन के लिए कोई सर्वोच्च सत्ता या ईश्वर अपेक्षित नहीं है। वैदिक धर्म को ईश्वर के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। नित्य एवं स्वयं-स्थित वेद जैमिनि तथा पूर्वमीमांसकों के प्रयोजनों की सिद्धि स्वयं कर देते हैं। जैमिनि जिस सीमा तक ईश्वर की उपेक्षा करते हैं, उस सीमा तक उसको अस्वीकृत नहीं करते।
वैदिक धर्म का पालन : आनन्द-प्राप्ति का साधन
वेदों अर्थात् श्रुति में वैदिक धर्म के पालन के स्पष्ट निर्देश हैं। इससे आनन्द की प्राप्ति होती है। यदि कहीं स्मृति तथा श्रुति में सहमति न हो, तो वहाँ स्मृति को उपेक्षणीय समझ लेना चाहिए। श्रुति के पश्चात् धार्मिक व्यक्तियों के आचरण का स्थान है। हिन्दू को वैदिक विधियों के अनुसार ही जीवन-यापन करना चाहिए। मुक्ति-प्राप्ति के लिए उसे समुचित अवसरों पर सन्ध्यादि नित्य कर्म तथा नैमित्तिक कर्म अवश्य करने चाहिए। ये कर्तव्य उसके लिए अनिवार्य हैं। यदि इन कर्तव्यों के पालन में उससे चूक होती है, तो वह प्रत्यवाय-दोष के पाप को प्राप्त होता है। किन्हीं विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए यह काम्य कर्मों का निष्पादन करता है। यदि वह निषिद्ध कर्मों से विरत रहता है, तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। अप्रतिबन्धित कर्तव्य-पालन से उसे मुक्ति प्राप्त होती है।
कुछ उत्तरकालीन मीमांसकों का मत है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों को ईश्वर अथवा परम आत्मा को हवि के रूप में समर्पित कर देना चाहिए। ये समर्पित कर्म ही मुक्ति के साधन हो जाते हैं। यदि यज्ञानुष्ठान बिना श्रद्धा-भक्ति की भावना के यान्त्रिक रूप से किये जाते हैं, तो वे मुक्ति-प्राप्ति में सहायक सिद्ध नहीं होते। कोई भले ही अनेक यज्ञ कर ले, यदि उन्हें सम्यक् अभिवृत्ति तथा समुचित रीति से सम्पन्न नहीं किया जाता, तो उसका हृदय-परिवर्तन असम्भव है। जो वस्तु यथार्थतः अपेक्षित है, वह औपचारिक यज्ञानुष्ठान न हो कर स्वार्थ, अहंकार तथा राग-द्वेष की बलि है।
अपूर्व का सिद्धान्त
यज्ञ का फल प्रदान करने वाला कोई दयालु ईश्वर नहीं, बल्कि अपूर्व है। यजमान को अपूर्व ही यज्ञ-फल प्रदान करता है। अपूर्व कर्म तथा कर्म-फल के बीच एक आवश्यक माध्यम है। अपूर्व अंदूर है। यह एक भावनात्मक अदृश्य शक्ति है जो कर्मजन्य होने के साथ-साथ कर्म-फल-प्रदाता भी है। जैमिनि का यही मत है। अन्य चिन्तकों ने इस मत की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है कि जड़ तथा अज्ञ अपूर्व कर्म-फल प्रदान करने में सर्वथा असमर्थ हैं। मीमांसा की पद्धति मेधावी या विचारशील व्यक्तियों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती। अतः उत्तरवतीं मीमांसकों ने ज्ञान। -शनैः इसमें ईश्वर को भी समाविष्ट कर लिया। उन्होंने उद्घोषित कर दिया कि बादि यज्ञ का सम्पादन परमात्मा के सम्मान में किया जाता है, तो इससे निःश्रेयस् की प्राप्ति होती है। तब तक ईश्वर या सर्वोच्च आत्मा अपूर्व में गति का संचार नहीं करता, तब तक यह क्रियाशील नहीं हो सकता। जो अपूर्व को क्रियाशील बनाता है, वह ईश्वर है।
आत्मा तथा इसका स्वरूप
आत्मा शरीर, इन्द्रिय तथा बुद्धि से भिन्न है। यह अनुभवकर्ता अथवा भोक्ता है। शाहीर अनुभवों का आवास है। इन्द्रियाँ अनुभव के करण हैं। आत्मा मन से संयुक्त हो कार ही द्रष्टा हो पाता है। आन्तरिक रूप से उसे सुख-दुःख का तथा बाह्य रूप से वृक्ष, नदी, वनस्पति आदि विषयों की उपस्थिति का अनुभव होता है।
आत्मा इन्द्रिय नहीं है; क्योंकि इन्द्रियों के आहत तथा नष्ट होने पर भी यह पूर्ववत् विद्यमान रहता है। शरीर भौतिक तत्त्वों से निर्मित है। द्रष्टा शरीर से पृथक् है। आत्मा शरीर का नियमन करता है। शरीर आत्मा का दास है। एक तत्त्व ऐसा है जो विभिन्न इन्द्रियों के क्रियाकलापों को संयोजित करता है। आत्मा ही वह तत्त्व है। वह सर्वव्यापी तथा नित्य है। आत्माओं की संख्या अगणित है।
यथार्थ आत्मा देहावसान के पश्चात् भी विद्यमान रहता है। यज्ञ करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। जैमिनि को मोक्ष में विश्वास नहीं है। उनका विश्वास स्वर्ग के अस्तित्व के प्रति है जो कर्म या यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होता है। वेद यजमान को परलोक में ज-फल की प्राप्ति के लिए आश्वस्त करता है।
उत्तरवर्ती मीमांसक
प्रभाकर और कुमारिल
जैमिनि ने स्वर्ग में आनन्द-प्राप्ति के लिए लोगों का पथ-प्रदर्शन तो किया; किन्तु आत्यन्तिक मुक्ति की समस्या के विषय में वे मौन ही बने रहे, लेकिन प्रभाकर तथा कुमारिल जैसे कुछ उत्तरकालीन लेखक अन्तिम मुक्ति की इस समस्या के प्रति उदासीन नहीं रह सके। इसका कारण यह था कि इस समस्या ने अन्य विचार-धाराओं के विचारकों को अपने प्रति आकृष्ट कर लिया था। प्रभाकर के अनुसार धर्माधर्म पुनर्जन्म के कारण हैं। इनके नितान्त तिरोभाव से शरीर का आत्यन्तिक उच्छेद हो जाता है। शरीर का यह आत्यन्तिक उच्छेद ही मुक्ति है। मनुष्य निषिद्ध तथा स्वर्गानन्द-प्रदायक कर्मों का परित्याग कर देता है। वह पूर्व-संचित कर्मी के नाश के लिए आवश्यक प्रयास करता है। वह आत्मनिग्रह का अभ्यास और अपना नियमन करता है। वह स्वयं में सद्गुणों का विकास करता है और आत्मज्ञान द्वारा स्वयं को पुनर्जन्म से मुक्त कर लेता है। कोई ज्ञान मात्र से मुक्त नहीं हो सकता; कर्म के दाध हो जाने पर ही मुक्ति सम्भव है। ज्ञान से आगामी पुण्य-पाप की निवृत्ति हो जाती है। एकमात्र कर्म से ही कोई आत्यन्तिक मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता। मुक्ति के आकांक्षी को कर्मों के प्रारम्भक राग-द्वेष को नष्ट करना होगा। मोक्ष सुख-दुःख का तिरोभाव है। यह निरतिशय आनन्द की स्थिति नहीं है; क्योंकि निर्गुण आत्मा को आनन्द का अनुभव भी नहीं होता। यह तो आत्मा का स्वाभाविक रूप मात्र है।
कुमारिल के दृष्टिकोण तथा अद्वैत वेदान्त की मान्यताओं में पर्याप्त साम्य है। कुमारिल के अनुसार वेद ईश्वर-कृत है। वे वेद को नाद-ब्रह्म की संज्ञा प्रदान करते हैं। उनके लिए मोक्ष एक भावात्मक अवस्था है। यह आत्म-साक्षात्कार है। कुमारिल के मतानुसार मुक्ति के लिए एकमात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उनकी मान्यता है कि आत्यन्तिक मुक्ति ज्ञान-कर्म-समुच्चय से ही सम्भव है।
जैमिनि के दर्शन का संक्षिप्त विवरण
जैमिनि के अनुसार वेद-विहित कर्म स्वर्ग-प्राप्ति के साधन हैं। कर्मकाण्ड वेदों का प्रमुख भाग है। निषिद्ध कर्म बन्धन के कारण हैं। आत्मा जड़त्व तथा चेतना का मिश्रित स्वरूप है अर्थात् वह जड़ भी है और चेतन भी। आत्माओं की संख्या अगणित है। आत्मा कर्ता, भोक्ता तथा सर्वव्यापी है। जगत् की सृष्टि-प्रक्रिया के प्रति जैमिनि को विश्वास नहीं है। वे स्वर्ग के आनन्द के विभिन्न स्तरों तथा सदाचार अर्थात् 'सत्यं वद' और 'धर्म चर' जैसे विधि-वाक्यों में विश्वास करते हैं।
जैमिनि के दर्शन की समीक्षा
पूर्वमीमांसा निरपेक्ष सत्ता तथा आत्मा और पदार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध की व्याख्या नहीं करता। अतः दर्शन की इस पद्धति को असन्तोषजनक तथा अपर्याप्त समझा जाता है। जगत् के प्रति इसका कोई दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं है। इसका केन्द्रीय स्वरूप यज्ञ का अनुष्ठान है। यह उसका सर्वाधिक सारगर्भित एवं मौलिक तत्त्व है। पाश करो तथा स्वर्ग के सुखों का उपभोग करो", जैमिनि की शिक्षाओं का सार इसी में गर्भित है; किन्तु यह उन विचारकों के लिए सन्तोषजनक नहीं है जो इस तथ्य से बारक्षित हैं कि स्वर्ग का सुखोपभोग अनित्य, अपूर्ण, ऐन्द्रिय तथा सांसारिक है।
वेदान्त-दर्शन
भूमिका
उत्तरमीमांसा अर्थात् दर्शन की वेदान्त शाखा के प्रवर्तक, भगवान् विष्णु के अवतार तथा पराशर ऋषि के पुत्र श्री व्यास को प्रणाम !
व्यास अर्थात् बादरायण के उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्त को परम्परागत इदर्शनों में अन्तिम स्थान दिया गया है; किन्तु वस्तुतः उसे सर्वोपरि स्थान दिया आना चाहिए।
उत्तरमीमांसा तथा उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में अत्यधिक साम्य है। वेदान्त का शाब्दिक अर्थ वेद का अन्त या इसका सारतत्त्व है। इसमें वेदों के अन्तिम भाग में वर्णित सिद्धान्त सन्निहित हैं। वेदों का अन्तिम भाग उपनिषद् हैं जो वेदों के मूलभूत कथ्य हैं।
भगवान् व्यास का ब्रह्मसूत्र
श्री व्यास ब्रह्म की व्याख्या करने वाले ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र अथवा वेदान्तसूत्र के प्रणेता हैं। ब्रह्मसूत्र को शारीरकसूत्र के नाम से भी जाना जाता है; क्योंकि यह सर्वोच्च तथा निर्गुण ब्रह्म के मूर्त रूप पर विचार करता है। ब्रह्मसूत्र हिन्दू-धर्म पर लिखे गये तीन सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थों (प्रस्थात्रयी) के अन्तर्गत आता है। इस प्रस्थानत्रयी के दो अन्य ग्रन्थ हैं उपनिषद् तथा श्रीमद्भगवद्गीता। व्यास ने वेदान्त के सिद्धान्तों को कुव्यवस्थित रूप दे कर उनमें बाह्य रूप से प्रतीत होने वाले विरोधाभासों का परिहार किया। ब्रहासूत्रों की संख्या ५५५ है। शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ, भास्कर, यादवप्रकाश, केशव, नीलकण्ठ, बलदेव और विज्ञानभिक्षु ब्रह्मसूत्र के प्रमुख भायकार हैं। इन्होंने अपने-अपने दृष्टिकोण से अपने भाष्यों की रचना की है और उनमें अपने-अपने दार्शनिक मतों की स्थापना की है। इस दार्शनिक विचारधारा के सर्वाधिक प्रख्यात आचार्य शंकराचार्य थे।
श्री व्यास ने वैशेषिक तथा सांख्य-मतों की आलोचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बौद्ध-धर्म के कई सम्प्रदायों तथा भागवत-धर्म को भी आलोचनात्मक विधि से देखा-परखा है।
समन्वय, अविरोध, साधन तथा फल ब्रह्मसूत्र के चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप एवं जगत् तथा जीव से इसके सम्बन्ध पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय में सांख्य, योग तथा वैशेषिक आदि विरोधी मतों की आलोचना की गयी है। इसमें इस मत के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्तियों के समुचित उत्तर भी दिये गये हैं। तृतीय अध्याय में ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के साधनों पर विचार किया गया है और चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के फलों का निरूपण है। इसमें जीव के देवयान-भार्ग द्वारा उस ब्रह्म तक पहुँचने का भी विवरण है जहाँ से प्रत्यावर्तन नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में जीवन्मुक्त के लक्षणों की भी समीक्षा की गयी है। प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं और कई एक सूत्रों से एक अधिकरण की संरचना हुई है।
प्रथम अध्याय के प्रथम पाँच सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। प्रथम सूत्र है-"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा।" इसका अर्थ है-अतः अब ब्रह्मविषयक जिज्ञासा। इस प्रथम सूत्र में वेदान्त की सम्पूर्ण पद्धति के उद्देश्य को एक शब्द 'ब्रह्मजिज्ञासा' में ही सुस्पष्ट कर दिया गया है। द्वितीय सूत्र है- "जन्माद्यस्य यतः।" इसका अर्थ है कि ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है जो सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का आदि कारण है। तृतीय सूत्र है-"शास्त्रयोनित्वात्।" इसका अर्थ है कि शास्त्र यथार्थ ज्ञान के साधन हैं। शास्त्रों का मूल कारण होने से ब्रह्म की सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाती है। चतुर्थ सूत्र में कहा गया है-"तत्तु समन्वयात्।" इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि ब्रह्मज्ञान किन्हीं अन्य स्वतन्त्र साधनों से नहीं, बल्कि शास्त्रों से ही सम्भव है; क्योंकि समस्त वैदिक ग्रन्थों का मुख्य अभिप्राय यही है। पंचम सूत्र में कहा गया है- "ईक्षतेर्नाशब्दम्।" इसका अर्थ है कि प्रकृति अथवा प्रधान में ईक्षण का अभाव है। अतः वह प्रथम कारण नहीं है। प्रधान शास्त्रों पर आधारित नहीं है। चतुर्थ अध्याय का अन्तिम सूत्र है-"अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्।" अर्थात् एतत्सम्बन्धी शास्त्रीय अनुदेशन के अनुसार मुक्तात्माओं का पुनः आगमन नहीं होता।
ब्रह्म, माया और जीव
निरपेक्ष ब्रहा तत्वों की सृष्टि के पश्चात् उनमें प्रविष्ट हो जाता है। यह सूर्य में स्थित हिरण्य पुरुष तथा आत्मा का प्रकाश है। यह नित्य-शुद्ध, स्वयं-प्रकाश, सद-चित्-आनन्द, अद्वितीय तथा भूमा (अनन्त तथा निरुपाधिक) है। आत्मा में स्थित तथा सबका आदि कारण है। यह मनुष्य की ब्रह्म जगत् का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। जिस प्रकार घट एतिका से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म भी जगत् से भिन्न नहीं है। ब्रह्य विना किसी विकार को प्राप्त हुए तथा बिना अपने स्वरूप से च्युत हुए जगत् में व्याप्त हो जाता है।
ब्रहा निष्कल, निर्विशेष, अकर्ता, राग-रहित, अनादि, अनन्त तथा अविकार्य है। 'मैं' तथा 'तुम' से सम्बन्धित चेतना से वह रहित है। वह एकमात्र यथार्थ सत्ता है। बाह्य जगत् से ब्रह्म का वही सम्बन्ध है जो सम्बन्ध वस्त्र से तन्तु का, मृत्तिका से घट का तथा मुद्रिका से स्वर्ण का है।
ब्रह्म पारमार्थिक सत्य, जगत् व्यावहारिक सत्य तथा स्वप्न के विषय प्रातिभासिक सत्य हैं।
माया
माया ईश्वर की शक्ति है और इसका कारण शरीर है। यह सत् को आवृत कर देती है। इसके कारण सत् असत् के रूप में अवभासित होता है। यह न तो सत् है, न असत् और न ही सत्-असत्। यह अनिर्वचनीय है। आवरण तथा विक्षेप इसकी दो शक्तियाँ हैं। माया की विक्षेप-शक्ति के कारण मनुष्य अपने यथार्थ दिव्य स्वरूप को विस्मृत कर चुका है। माया की विक्षेप-शक्ति के कारण ही जगत् अवभासित होता है।
जीव
जीव पंचकोशों में आबद्ध है। ये कोश प्याज की भाँति हैं। अन्नमय-कोश, प्राणमय-कोश, मनोमय-कोश विज्ञानमय कोश तथा आनन्दमय-कोश-ये पंचकोश हैं। प्रथम कोश से स्थूल शरीर की, उत्तरवर्ती तीन कोशों से सूक्ष्म शरीर की तथा अन्तिम आनन्दमय-कोश से कारण शरीर की संरचना होती है। जीव को ध्यान द्वारा अपने सभी कोशों का अतिक्रमण कर उस सर्वोच्च सत्ता से तादात्म्य स्थापित कर लेना चाहिए जो पंचकोशों से परे है। केवल इसी स्थिति में उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है।
जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति-जीव-चेतना की ये तीन अवस्थाएँ हैं। चतुर्थ अवस्था तुरीयावस्था है जो अधिचेतनात्मक अवस्था है। तुरीय ब्रह्म और अवस्था-त्रय का मूक साक्षी है। जीव को प्रथम तीन अवस्थाओं का अतिक्रमण कर चतुर्थ तुरीयावस्था में समाहित हो जाना चाहिए। तभी वह सर्वोच्च सत्ता से एकत्व स्थापित कर सकता है।
अविद्या जीव का कारण शरीर है। जीव अविद्या के कारण स्वयं को शरीर, मन तथा इन्द्रियों में अध्यारोपित करता है। जिस प्रकार भ्रम के कारण गोधूलि में रज्जु में सर्प का भास होता है, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान के कारण जीव को शरीर में आत्मा का भास होता है। जिस क्षण जीव सर्वोच्च ब्रह्म के विषय में वेदान्तप्रोक्त विचार, मनन तथा ध्यान के माध्यम से चरम सत्य के सम्यक् बोध द्वारा स्वयं आरोपित अज्ञान से मुक्त हो जाता है, उसी क्षण उसके अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। इस स्थिति में जीव तथा जागतिक प्रपंच का ब्रह्म के साथ पुनः तादात्म्य-स्थापन हो जाता है, जीव को अमरत्व तथा शाश्वत आनन्द की सम्प्राप्ति हो जाती है और वह अन्ततः ब्रह्म अर्थात् आनन्द-सिन्धु में विलीन हो जाता है।
बादरायण जीवन्मुक्ति में विश्वास करते हैं।
प्रख्यात वेदान्त-वाक्य
वेदान्त के प्रख्यात वाक्य निम्नवत् हैं :
● एकमेवाद्वितीयम् यथार्थ सत्ता एक और अद्वितीय है।
● ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः- ब्रह्म की पारिमार्थिक सत्ता है, जगत् मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है।
● सर्वं खल्विदं ब्रह्म-निश्चित रूप से यह सब-कुछ ब्रह्म ही है।
● सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म-ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है।
● ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति -ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म हो जाता है।
● शान्तं शिवं अद्वैतम्-ब्रह्म शान्त, शिव और अद्वितीय है।
● अयम् आत्मा शान्तः यह आत्मा शान्त है।
● असंगो अयम् पुरुषः यह पुरुष असंग है।
● शान्तं अजरं अमृतं अभयं परम-यह ब्रह्म शान्त, अजर, अमर, निर्भय और सर्वोच्च है।
आप सब लोग वेदान्त-दर्शन के सत्य से अवगत हों! आप सब लोगों को अभेद के आनन्द का साक्षात्कार हो ! आप सब लोग जीवन्मुक्त हों!
द्वादश अध्याय
हिन्दू-दर्शन-२
(वेदान्त-शाखा)
प्रस्तावना
व्यास का ब्रह्मसूत्र वेदान्त-दर्शन का मूलाधार है। विभिन्न भाष्यकारों ने इन सूत्रों की व्याख्या विभिन्न रूपों में की है और इन व्याख्याओं के कारण दर्शन की कई-एक शाखाओं का उद्भव हुआ है। श्री शंकर का केवलाद्वैत-दर्शन, श्री रामानुजाचार्य को विशिष्टाद्वैत-दर्शन, श्री मध्वाचार्य का द्वैत-दर्शन, श्री निम्बार्काचार्य का भेदाभेद-दर्शन, श्री वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत-दर्शन, श्री चैतन्य का अचिन्त्य-भेदाभेद-दर्शन तथा श्री मिकेन्दर का सिद्धान्त-दर्शन जैसी विचारधाराएँ इन्हीं विभिन्न व्याख्याओं से आविर्भूत हुई हैं।
ईश्वर, जगत् तथा जीव-इस त्रयी का तत्त्वार्थ-निरूपण ही दर्शन की प्रत्येक शाखा का प्रयोजन है। दर्शन की अनेकानेक विचारधाराएँ सत्यान्वेषण के विभिन्न प्रयास हैं।
विभिन्न मतों से सम्बन्धित विभिन्न आचार्य विभिन्न सम्प्रदायों तथा विचारधाराओं के प्रवर्तक हुए। इन विचारधाराओं के अनुयायियों ने अपने सिद्धान्तों के अनुरूप वेदान्त-सूत्रों की व्याख्या के माध्यम से अपने मतों की प्रामाणिकता की सिद्धि के प्रयास किये। अपने इस अभियान में उन्होंने अपनी मान्यताओं को पुरातन शास्त्रीय परम्पराओं पर आधारित तथा इनसे विधिवत् विकसित होने का दावा प्रस्तुत किया।
श्रुति : समस्त विचारधाराओं का सामान्य आधार
वेदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों पर आधारित हैं। उपनिषदों, वेदान्तसूत्रों तथा भगवद्गीता को प्रामाणिक शास्त्रों के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उन्हें प्रस्थानत्रयी ग्रन्थ की संज्ञा की गयी है। ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के विषय में वेदान्तसूत्रों के विभिन्न आध्यकारों के पृथक् पृथक् मत हैं; किन्तु वे अपनी स्थापनाओं को श्रुतियों के सर्वोच्च प्रमाणों पर ही प्रतिष्ठित करते हैं। इन मतों में से किसी भी मत को अस्वीकार करना स्वयं श्रुतियों को अस्वीकार करना है।
तत्त्व-विज्ञान के तीन प्रमुख सिद्धान्त द्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत
श्री शंकर, श्री रामानुज तथा श्री मध्व वेदान्त-सूत्र के सर्वाधिक उल्लेखनीय भाष्यकार हैं। इन भाष्यकारों ने अपने-अपने स्वतन्त्र मतों अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की स्थापना के प्रयास किये हैं। अपने भाष्य की रचना करते समय शंकर के समक्ष हिन्दुत्व पर तत्कालीन अन्ध-कर्मकाण्ड के विषाक्त प्रभाव के विरुद्ध अपने संघर्ष का प्रयोजन स्पष्ट था।
द्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्वैत तत्त्वमीमांसा की तीन प्रमुख विचारधाराएँ हैं जो चरम सत्य अर्थात् परब्रह्म के साक्षात्कार की विधियों के विभिन्न चरण हैं। ये योग-रूपी सोपान की दण्डिकाएँ हैं जो परस्पर विरोधी न हो कर एक-दूसरे की अनुपूरक हैं। इन चरणों को आध्यात्मिक अनुभवों की श्रेणीबद्ध श्रृंखला में समस्वर विधि से व्यवस्थित किया गया है। द्वैत, विशिष्टाद्वैत तथा शुद्धाद्वैत का पर्यवसान अन्ततः अद्वैत-वेदान्त-प्रोक्त निरपेक्ष सत्ता अर्थात् लोकोत्तर त्रिगुणातीत अनन्त ब्रह्म में ही होता है।
"मनुष्य ईश्वर का दास है," मध्व ने अपनी उद्घोषणा के साथ अपने द्वैत-दर्शन की स्थापना की और रामानुज के इस कथन के साथ अपने विशिष्टाद्वैत-दर्शन का प्रतिपादन किया कि "जीव ईश्वर का स्फुलिंग है।" शंकर ने कहा- "मनुष्य ब्रह्म से अभिन्न अथवा नित्य आत्मा है।" अपने इसी सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने केवलाद्वैत-दर्शन की स्थापना की।
द्वैती भगवान् का सेवक बन कर उसकी सेवा करना चाहता है। वह उसके साथ खेलना और मिश्री का रसास्वादन करना चाहता है। विशिष्टाद्वैती भगवान् नारायण के सामीप्य में रह कर दिव्य भाव का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। वह स्वयं को भगवान् में विलीन कर उससे तद्रूप हो जाना नहीं चाहता। वह अपने-आपको एक स्फुलिंग के रूप में ही बनाये रखना चाहता है। ज्ञानी ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित कर स्वयं मिश्री हो जाना चाहता है।
लोगों की प्रकृति तथा क्षमता में वैभिन्य होता है; अत विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का होना भी आवश्यक है। अद्वैत-दर्शन सर्वोच्च सोपान है। दैती या विशिष्टाद्वैती अन्ततः केवलाद्वैती हो जाते हैं।
ब्रह्म की विभिन्न अवधारणाएँ यथार्थ सत्ता के संस्पर्श की
विभिन्न विधियाँ
निम्बार्काचार्य शंकर, रामानुज, मध्य तथा अन्य दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित ब्रहा-सम्बन्धी अवधारणाओं में समन्वय स्थापित करते हैं। वे यह सिद्ध करते हैं कि अपनी-अपनी विधि से ब्रह्म के विशिष्ट पक्षों के सम्बन्ध में प्रतिपादित इन सबकी अवधारणाएँ निर्धान्त हैं। शंकर ने यथार्थ का ग्रहण उसके लोकोत्तर पक्ष के सन्दर्भ में किया है, जब कि रामानुज ने उसे मुख्यतः उसके अन्तर्यामित्व के सन्दर्भ में ग्रहण किया है। निम्बार्क ने विभिन्न भाष्यकारों के विभिन्न विचारों में समायोजन की व्यवस्था की है।
श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य और श्री निम्बार्काचार्य महान् पुरुष थे। हम यह नहीं कह सकते कि रामानुज की अपेक्षा शंकर या निम्बार्क की अपेक्षा वल्लभ महान् थे। ये सभी अवतार-पुरुष थे। इनमें से प्रत्येक एक काल-विशेष तथा विकास के एक निश्चित चरण में विद्यमान एक विशिष्ट जन-समुदाय के निमित्त आवश्यक सिद्धान्तों के प्रशिक्षण तथा प्रसार के एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ था। दर्शन की प्रत्येक विचारधारा आवश्यक है। एक विशेष प्रकृति के लोगों के लिए प्रत्येक दर्शन अनुकूल तथा उपयुक्त होता है। ब्रह्म-सम्बन्धी विभिन्न धारणाएँ यथार्थ सत्ता के तत्त्वार्थग्रहण की विभिन्न विधियाँ मात्र हैं। बद्ध जीव के लिए अनन्त अथवा असीम आत्मा या चरम सत्ता के स्वरूप के सम्बन्ध में तत्क्षण किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाना अत्यन्त कठिन ही नहीं, असम्भव भी है और इससे भी अधिक दुष्कर है उपयुक्त शब्दों में इसकी अभिव्यक्ति।
श्री शंकर के सर्वोच्च केवलाद्वैत-दर्शन का ज्ञान सबके लिए सम्भव नहीं है। इसके पूर्व कि मन श्री शंकर के अद्वैत वेदान्त के निहितार्थ ग्रहण का एक सक्षम साधन हो जाये, इसे सम्यक् विधि से अनुशासित करना आवश्यक है।
सभी आचार्यों को मेरा प्रणाम! उनकी महिमा अक्षुण्ण हो! हम सब लोगों के शीश पर उनका आशिष-वर्षण होता रहे!
शंकर का अद्वैत-दर्शन
प्रस्तावना
अद्वैत का विधिवत् प्रतिपादन सर्वप्रथम श्री शंकर के परम गुरु गौड़पाद ने किया। गोविन्द गौड़पाद के तथा शंकर गोविन्द के शिष्य थे। गौड़पाद ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ माण्डूक्यकारिका' में अद्वैत वेदान्त के केन्द्रस्थ अनुदेशन को व्याख्यायित किया है; किन्तु यह शंकर ही थे जिन्होंने अद्वैत-दर्शन को एक निर्णायक तथा रमणीय रूप में चित्रांकित करने के पश्चात् ही अपनी तूलिका को विश्राम लेने दिया। मुख्य उपनिषदों, वेदान्त-सूत्र तथा भगवद्गीता के सुविचारित अध्ययन से आपको इनके अद्वैत वेदान्त का स्पष्ट बोध हो जायेगा। 'वेदान्त-सूत्र' के शांकर-भाष्य को 'शारीरिक-भाष्य' कहते हैं।
शंकर के उपदेशों को एक पद्य के अर्धांश में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और वह अर्धांश है -"ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रहौव नापरः।" अर्थात् ब्रह्म सत्य है, ज्ञात् मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अभिन्न है। यही उनके दर्शन का सारतत्त्व है।
शंकर द्वारा अनुदेशित अद्वैत केवलाद्वैत अर्थात् निरपेक्ष अद्वैत है। उनके अनुसार यह सब-कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म एक-रस है, भेद और नानात्व नितान्त मायिक हैं।
ब्रह्म अद्वितीय है
आत्मा स्वतःसिद्ध है। बाह्य प्रमाणों से इसकी सिद्धि नहीं होती। आत्मा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अस्वीकार किया जाने वाला आत्मा स्वयं अस्वीकार करने वाले का ही सारभूत तत्त्व है। आत्मा ज्ञान की समस्त विधाओं, पूर्व-धारणाओं तथा प्रमाणों का अधिष्ठान है। आत्मा आभ्यन्तर भी है और बाह्य भी, पूर्व भी है और पश्च भी, दक्षिण भी है और वाम भी एवं ऊर्ध्व भी है और अधः भी।
अदृश्य होने के कारण ब्रह्म पदार्थ या द्रव्य नहीं है, अतः उपनिषदें उसे 'नेति नेति' की उद्घोषणा के माध्यम से ही व्याख्यायित करती हैं; किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म एक निषेधात्मक प्रत्यय या एक आध्यात्मिक अमूर्तता या अनस्तित्व या रिक्ति है। वह तो आप्तकाम, अनन्त, अविकार्य, स्वयंस्थित, आनन्दस्वरूप, भानस्वरूप तथा भूमास्वरूप है। वह स्वरूप का सारतत्त्व है। वह प्रमाता का सारतत्त्व, देश, तुरीय एवं साक्षी है।
शंकर का परब्रह्म निवैयक्तिक, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, अविकार्य, नित्य तथा अकर्ता है। वह प्रयोजन-शून्य तथा इच्छा-रहित है। वह सार्वकालिक साक्षी प्रमाता है। इन्द्रियातीत होने के कारण वह इन्द्रियों का विषय कदापि नहीं हो सकता। वह अद्वय एवं अद्वितीय है। वह नितान्त असंग एवं बहिरंग तथा अन्तरंग भेदों से रहित है। ब्रह्म का निर्वचन असम्भव है; क्योंकि निर्वचन की प्रक्रिया में विभेदीकरण निहित रहता है। ब्रह्म की तुलना केवल ब्रह्म से ही की जा सकती है, किसी अन्य से नहीं। ब्रह्म में तत्त्वात्मक या गुणात्मक भेद नहीं है। सत्-चित्-आनन्द उसका गुण न हो कर उसका स्वरूप है।
शंकर का ब्रह्म निराकार है। माया-वच्छिन्न हो कर ही वह साकार या सगुण ब्रह्म होता है।
सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रम्ह पृथक् पृथक् दो ब्रह्म नहीं हैं। इन दोनों के बीच वैषम्य, प्रतिवाद तथा विरोध के दर्शन नहीं होते। भक्त की पावन पूजा के लिए वही निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म की भाँति प्रतीत होता है। दो दृष्टिकोणों से देखा जाने वाला यह सत्य एक ही है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखने पर निर्गुण ब्रह्म परब्रह्म तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने पर सगुण ब्रह्म अपरब्रह्म है।
जगत् : एक व्यावहारिक सत्ता
शंकर के मतानुसार जगत् मिथ्या नहीं है। यह व्यावहारिक सत्ता तथा ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है। जगत् माया या अविद्या की सृष्टि है। माया के कारण अविकार्य ब्रह्म विकारशील जगत् प्रतीत होने लगता है। माया ईश्वर की एक रहस्यमयी अनिर्वचनीय शक्ति है जो सत् को आवृत्त कर स्वयं को असत् के रूप में अभिव्यक्त किया करती है। माया सत् (भाव-रूपा) नहीं है, क्योंकि यह नित्य सत्ता अर्थात् ब्रह्म के ज्ञान के पश्चात् लुप्त हो जाती है; किन्तु यह असत् (अभाव-रूपा) भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाता तब तक इसकी सत्ता की प्रतीति होती रहती है। ब्रह्म पर जगत् का अध्यारोप अविद्या के कारण होता है।
जीव का स्वरूप तथा मोक्ष के साधन
शंकर का जीव अथवा वैयक्तिक आत्मा सापेक्ष अर्थात् व्यावहारिक रूप से ही सत्य है। वैयक्तिकता से वह तभी तक ग्रस्त रहता है, जब तक वह अविद्या के कारण असत् उपाधि से सम्प्रयुक्त रहता है। अविद्या से सम्मोहित हो कर जीव शरीर, मन तथा इन्द्रियों से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसी अविद्या या अज्ञान के कारण वह विचार, कर्म तथा भोग करता है। यथार्थतः वह ब्रह्म अथवा निरपेक्ष सत्ता से भित्र नहीं हैं। "तत् त्वम् असि" अर्थात् "तुम वही हो" यह उपनिषदों की सुस्पष्ट उद्घोषणा है। जिस प्रकार जल का बुलबुला फूट कर समुद्र के साथ एक हो जाता है और जिस प्रकार घट के टूटने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होने पर जीव अर्थात् आनुभविक आत्मा ब्रह्म के साथ एकास हो जाता है। जब जीव में ज्ञानोदय होता है, तब वह अपने पृथक् वैशिष्ट्य तथा सीमितता से मुक्त हो कर अपने तात्त्विक स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। वह स्वयं को आनन्द-सिन्धु में अन्तर्लयित कर लेता है और जीवन-सरिता का निरपेक्ष सत्ता के सिन्धु में अन्तर्भाव हो जाता है। यही चरम सत्य है।
जीव तथा ब्रह्म के बीच वैभिन्य-दर्शन एक भ्रान्त धारणा है। शंकर के अनुसार इस भ्रान्त धारणा की निवृत्ति के पश्चात् जीव का ब्रह्म में आत्यन्तिक अन्तर्लयन ही सांसारिक प्रपंच से मुक्ति है। शंकर कर्म तथा भक्ति को ज्ञान का साधन मानते हैं। वे ज्ञान को ही मोक्ष की संज्ञा प्रदान करते हैं।
विवर्तवाद अर्थात् अध्यारोप का सिद्धान्त
शंकर के अनुसार जगत् की केवल व्यावहारिक सत्ता है। उन्होंने विवर्तवाद अर्थात् आभास अध्यारोप (अध्यास) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। जिस प्रकार गोधूलि में रज्जु में सर्प का अध्यास या आभास होता है, उसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा में संसार एवं देह का अध्यारोप होता है। रज्जु के ज्ञान से इसमें अध्यस्त सर्प के भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्म अर्थात् नित्य सत्ता के ज्ञान से शरीर एवं जगत् के भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण को अपने स्वरूप को विकृत करने की आवश्यकता नहीं होती। रज्जु में सर्प का आभास मिथ्या प्रतीति मात्र है। यहाँ रज्जु का सर्प में इस प्रकार रूपान्तरण नहीं हुआ है जिस प्रकार दूध का दही में होता है। ब्रह्म नित्य तथा अविकार्य है; अतः यह स्वयं को जगत् में रूपान्तरित नहीं कर सकता। माया ब्रह्म की विलक्षण तथा रहस्यमयी शक्ति है। वह इसी माया के संयोग में कारण या स्रष्टा बनता है।
रज्जु के ज्ञान से आपके भय की निवृत्ति हो जाती है और आप उस स्थान से पलायित नहीं होते। इसी प्रकार जब आपको नित्य तथा निर्विकार ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तब आप नाम-रूपात्मक जगत् से प्रभावित नहीं होते। जब शाश्वत सत्ता अर्थात ब्रह्म के ज्ञान से अविद्या अथवा अज्ञान का आवरण विच्छिन्न हो जाता है और जब अविनाशी एवं यथार्थ सत्ता के ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तब आप अपनी मूलभूत दिव्य प्रदीप्ति तथा गरिमा को प्राप्त कर ज्योतिर्मय हो उठते हैं।
अद्वैत : एक अद्वितीय दर्शन
शंकराचार्य का अद्वैत-दर्शन एक उद्दात्त, भव्य तथा अद्वितीय दर्शन है। यह सूक्ष्म तार्किकता तथा निर्भीक दर्शन की वैचारिक पद्धति है। यह अत्यन्त मनोरंजक, प्रेरणाप्रद तथा समुन्नत दर्शन है। निर्भीकता, गहनता तथा सूक्ष्म वैचारिकता में इसके समक्ष किसी भी दर्शन का टिक पाना असम्भव है। शंकर का दर्शन समृद्ध तथा पूर्ण है।
शंकर एक प्रचण्ड तथा चमत्कारपूर्ण मेधा के स्वामी थे। वे तर्क-शास्त्र में निष्णात थे। वे उच्चकोटि के गम्भीर चिन्तक तथा सन्त थे। उन्हें उच्चतम सिद्धियाँ प्राप्त थीं। वे भगवान् शिव के अवतार थे। उनका दर्शन पूर्व तथा पश्चिम के असंख्य लोगों के लिए सान्त्वना, शान्ति तथा प्रकाश का स्रोत सिद्ध हुआ। पाश्चात्य चिन्तक श्री शंकर के चरण-कमलों पर नतमस्तक होते हैं। उनका दर्शन पूर्व तथा पश्चिम के असंख्य लोगों के लिए सान्त्वना, शान्ति तथा प्रकाश का स्रोत सिद्ध होता आ रहा है। सर्वाधिक सन्तप्त लोगों के सन्ताप तथा उनकी पीड़ाओं का शमन उनके दर्शन से हुआ है। अनेक लोगों को आशा, हर्ष, सम्बोधि, पूर्णत्व, स्वातन्त्र्य तथा शान्ति की प्राप्ति हुई है। शकंर के दर्शन ने समस्त संसार से प्रशंसा अर्जित की है।
श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत-दर्शन
प्रस्तावना
ब्रह्म के अद्वैत या एकत्व को एक विशिष्ट विधि से प्रतिपादित करने के कारण इस दर्शन को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। इसके अनुसार केवल ईश्वर ही सत् है। यह समस्त दृश्यमान जगत् उसकी अभिव्यक्ति या उसका गुण है। श्री रामानुज के ईश्वर या भगवान् नारायण एक जटिल तथा व्यवस्थित तत्त्व हैं जो एक हो कर भी विशिष्ट हैं। अतः इस दर्शन का नाम विशिष्टाद्वैत है।
शंकर के अनुसार समस्त विकार या प्रपंच असत् या अनित्य हैं। इसका कारण अविद्या या अज्ञान है। रामानुज के मतानुसार गुण यथार्थ तथा नित्य हैं; किन्तु इनका नियन्त्रण ब्रह्म द्वारा होता है। गुणों की यथार्थ सत्ता ब्रह्म के एकत्व की असन्दिग्धता को प्रतिबन्धित नहीं कर सकती; क्योंकि गुणों की पृथक् सत्ता नहीं है। वे एक ही ब्रा के प्रकार, रूप तथा नियम अर्थात् नियन्त्रित पक्ष हैं।
विशिष्टाद्वैत के नाम से प्रख्यात रामानुज का दर्शन विशिष्ट अर्थात् सविशेष अद्वैत है। यह नानात्व को स्वीकार करता है। रामानुज का ब्रह्म अनेक विदचिद् रूपों में विद्यमान है। अतः उनके दर्शन को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। यह एक वैष्णव-दर्शन है। रामानुज-सम्पदाय को श्री-सम्प्रदाय के नाम से जाना जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव होते हैं। रामानुज ने वैष्णव-मत के दर्शन को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उनके धार्मिक मत को श्री वैष्णव-गत कहा जाता है; क्योंकि श्री अर्थात्, देवी लक्ष्मी को जीवात्माओं की मुक्ति का महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा गया है।
श्री शंकर का दर्शन बहुसंख्यक जनों के लिए अत्यन्त गहन, सूक्ष्म तथा अमूर्त है. किन्तु जिन लोगों में भक्ति-भाव का प्राधान्य है, उन लोगों के लिए श्री रामानुज का दर्शन उपयुक्त एवं सुविधाजनक है। श्री रामानुज की दर्शन-पद्धति में ईश्वर के जीव जगत् अर्थात् चित् तथा अचित्-ये दो प्रकार हैं। ये उससे उसी प्रकार सम्बद्ध है इसे शरीर आत्मा से सम्बद्ध है। ईश्वर से पृथक् इनकी कोई सत्ता नहीं है। ये उसमें समाश्रित गुणों की भाँति विद्यमान रहते हैं। जगत् तथा जीव उसके शरीरभूत हैं। ईश्वर उनका अन्तर्यामी तथा नियन्त्रक यथार्थ तत्त्व है। चित् तथा अचित् अर्थात् जीव तथा इनाति उसका शरीर हैं। ये दोनों तत्त्व उसके अधीन हैं। इन्हें विशेषण तथा गुण कहा जाता है। ईश्वर विशेष्य अथवा सविशेष है।
विशिष्टाद्वैत-मत की विकास-कथा
विशिष्टाद्वैत-मत एक पुरातन मत है। सर्वप्रथम बोधायन ने ईसा से चार सौ वर्ष पूर्व रचित अपनी वृत्ति में इसका प्रतिपादन किया था। यह रामानुज द्वारा प्रतिपादित मत के अनुरूप है। रामानुज ने ब्रह्मसूत्रों के अपने भाष्य में बोधायन का ही अनुसरण किया।
भक्ति-मार्ग में वैयक्तिक ईश्वर अर्थात् सगुण-साकार ईश्वर की उपासना की जाती है। भक्त-जन वासुदेव अर्थात् नारायण के प्रति अपने भक्ति-भाव को विकसित करते हैं। सगुण-साकार ईश्वर के उपासकों को भागवत कहा जाता है। उनके अपने शाख हैं जिन्हें पांचरात्र-आगम कहा जाता है और जिन्हें वे लोग उपनिषदों के समकक्ष ही मानते हैं। द्वादश आलवार सन्तों की रचनाओं से दक्षिण भारत में भक्ति-आन्दोलन को पर्याप्त बल मिला। इन आलवार सन्तों द्वारा रचित चालीस सहस्र स्तोत्रों के सकलन को 'नालायिर प्रबन्धम्' कहते हैं।
तदनन्तर नाथमुनि, यामुनाचार्य तथा रामानुजाचार्य नामक वैष्णव आचार्यों का आगमन हुआ। ये लोग महान् पण्डित थे। इन लोगों ने अपनी आस्थाओं तथा अपने आवरण को एक दार्शनिक आधार तथा रंजकता प्रदान की। आलवारों के लिए ईश्वर-साक्षात्कार का एकमात्र साधन भक्ति ही थी; किन्तु भक्ति के साथ उन्होंने ज्ञान तथा कर्म को भी समन्वित कर लिया। वे ज्ञान तथा कर्म को भी ईश्वर-साक्षात्कार का साधन मानते थे। उनका उद्देश्य वेदों, उपनिषदों तथा गीता का 'तमिल प्रबन्ध' से सामंजस्य स्थापित करना था। उन्होंने तमिल प्रबन्धों की व्याख्या उपनिषदों तथा गीता के परिप्रेक्ष्य में ही की। अतः उन्हें उभय-वेदान्ती कहा जाता है। रामानुज वेदों, उपनिषदों तथा तमिल प्रबन्धों को अपने दर्शन का स्रोत मानते हैं। इसी कारण उनकी दर्शन-पद्धति को उभय-वेदान्त की संज्ञा प्रदान की गयी है।
नाथ मुनि ने तमिल प्रबन्धों को वेदों तथा उपनिषदों के स्तर तक समुन्नत किया और यामुनाचार्य ने अपने उत्तराधिकारी रामानुज के दर्शन की स्थापना के लिए आधारशिला प्रदान की। 'ब्रह्मसूत्र' पर रामानुज ने जो भाष्य लिखा, उसे 'श्री-भाष्य' कहते हैं। उन्होंने भगवद्गीता पर भी एक भाष्य की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने वेदान्त-सार, वेदान्त-संग्रह तथा वेदान्त-दीप नामक तीन अन्य ग्रन्थों की भी रचना की। दर्शन की विशिष्टाद्वैत-पद्धति के ये प्रमुख ग्रन्थ माने जाते हैं।
रामानुज प्रत्यक्ष, अनुमान तथा श्रुति को ज्ञान का प्रामाणिक स्रोत मानते हैं। ब्रह्मज्ञान के लिए वेद तथा स्मृतियाँ एकमात्र स्वतन्त्र एवं अधिकृत प्रामाणिक आधार हैं। वे सत्कार्यवाद तथा परिणामवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं जिसके अनुसार कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है।
रामानुज का ब्रह्म : साकार तथा सगुण ईश्वर
रामानुज के मतानुसार जो-कुछ भी है, वह ब्रह्म ही है; किन्तु ब्रह्म के स्वभाव में सामंजस्य तथा एकरसता नहीं है। इसके अन्तर्गत अनेकत्व के तत्त्व निहित हैं जिसके फल-स्वरूप वह स्वयं को वैविध्यपूर्ण जगत् के रूप में अभिव्यक्त करता है। रामानुज का ब्रह्म स्वरूपतः एक सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा जगन्नियन्ता वैयक्तिक परमात्मा है। वह जगत् में व्याप्त तथा जगत् उससे अनुप्राणित है। इस प्रकार पर निर्गुण ब्रह्म तथा अपर सगुण ब्रह्म के बीच एवं ब्रह्म तथा ईश्वर के बीच किसी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। रामानुज का ब्रह्म सविशेष तथा सगुण ब्रह्म है।
रामानुज का ब्रह्म निर्गुण-निरपेक्ष नहीं है। वह सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, असीम प्रेम आदि गुणों से सम्पन्न वैयक्तिक अथवा सगुण ईश्वर है। ईश्वर सगुण है। वेदोक्त निर्गुण ब्रह्म से तात्पर्य है कि वह शोक, दुःख, मरणशीलता, विकार एवं जरा आदि हेय गुणों से सर्वथा रहित है।
ईश्वर सभी वस्तुओं में अनुस्यूत है। वह आत्मा का सार-तत्त्व है। वह अन्तर्यामी तथा आत्मा से अभिन्न है। वह विभु, परम सत्ता तथा शुभ गुणों से सम्पत्र है। यह सच्चिदानन्द-स्वरूप है। जगत् तथा आत्मा उस पर आधारित हैं। वह इस विश्व तथा आत्माओं का मूलाधार है। ईश्वर जगत् का नियंता है। जीव अर्थात् आत्मा नियम्य अर्थात् शेष है।
ईश्वर अन्तर्यामी, विश्वातीत तथा अविकार्य है। प्रलय काल में समस्त विश्व उसमें विलीन हो जाता है। सृष्टि के समय जगत् का आविर्भाव होता है; किन्तु इससे उसका यथार्थ स्वरूप प्रभावित नहीं हो पाता। रामानुज के ब्रह्म में स्वगत-भेद है। पर (वासुदेव), व्यूह (संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध), विभव, अर्च तथा अन्तर्यामी-ईश्वर के ये पंच स्वरूप हैं। वह चिद्-अचिद्-विशिष्ट एक संश्लिष्ट समग्रता है।
रामानुज का ईश्वर नारायण है जो अपनी शक्ति अथवा सहधर्मिणी के साथ बैकृष्ठ में निवास करता है। लक्ष्मी समृद्धि की देवी हैं। वे दिव्य मातृ-स्वरूपा हैं। वे अपने पतिदेव के समक्ष मनुष्यों का पक्ष-समर्थन करती हैं। वे उनको भक्त जनों का परिचय दे कर उनको मोक्ष प्रदान करवाती हैं। विशिष्टाद्वैत-मत में लक्ष्मी को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है।
जगत् : ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ अंश
अपने विविध रूपों एवं जीवात्माओं-सहित जगत् असत् माया न हो कर ब्रह्म हे स्वरूप का एक यथार्थ अंश है। यह ईश्वर का शरीर है। पदार्थ सत् है। यह अचित् अर्थात् चेतना-शून्य द्रव्य है। यह वास्तविक परिणाम या विकास को प्राप्त हुआ करता है। प्रलय-काल में ईश्वर के प्रकार के रूप में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। अतः यह नित्य, किन्तु परतन्त्र है। इसका नियमन ईश्वरेच्छा द्वारा होता है। यह न तो शुभ है, न अशुभ। यह जीवों के कर्मानुसार सुख-दुःख का कारण हुआ करता है। यह जीवों के आनुभविक विषयों का स्रष्टा है।
सत्व, रजस् तथा तमस्-प्रकृति में ये तीन गुण हैं; किन्तु शुद्ध तत्त्व में केवल सत्व ही है। यह शुद्ध पदार्थ है। यह ईश्वर के शरीर की संरचना का संघटक तत्त्व है। इसे ईश्वर की नित्य-विभूति कहा जाता है। व्याकृत जगत् उसकी लीला-विभूति है।
आत्मा : एक विशिष्ट वैयक्तिक सत्ता
चेतन होने के कारण आत्मा पदार्थ की अपेक्षा परमात्मा का एक उच्चतर रूप है। इसमें परमात्मा का सारतत्व निहित है। रामानुज के अनुसार परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृति-ये तीनों नित्य हैं। आत्मा स्वयं चेतन, निर्विकार, निरवयव तथा अणु रूप है। आत्माएँ अनेक हैं। रामानुज का वैयक्तिक आत्मा यथार्थतः वैयक्तिक है। यह पूर्णतः यथार्थ तथा परमात्मा से सर्वथा भिन्न है। ब्रह्म से उद्भूत एवं ब्रह्म में अन्तर्निहित होते हुए भी इसकी एक पृथक् वैयक्तिक सत्ता है और यह पार्थक्य सार्वकालिक है।
जीवात्मा के तीन वर्ग
रामानुज के अनुसार आत्मा के नित्य, मुक्त तथा बद्ध-ये तीन वर्ग होते हैं। नित्य जीव सर्वदा से मुक्त रहे हैं। ये नित्य मुक्त जीव सर्वथा स्वतन्त्र होते हैं तथा नारायण के सान्निध्य में वैकुण्ठ में वास करते हैं। जहाँ तक मुक्त जीवों का सम्बन्ध है, वे सांसारिकता में लिप्त रहने के पश्चात् अब मुक्त हो कर नारायण का सामीप्य-लाभ कर चुके हैं। बद्ध जीव जागतिक प्रपचों में संलग्न रहते हुए मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे जब तक मुक्त नहीं हो जाते, तब तक उन्हें अनेक बार जन्म-ग्रहण करना पड़ता है।
परमात्मा अंशी तथा वैयक्तिक आत्मा अर्थात् जीव उसका अंश है जो उस अग्नि-पिण्ड का एक स्फुलिंग मात्र है। जो सम्बन्ध दाड़िम के किसी समग्र फल तथा उसके दानों के बीच है, वही सम्बन्ध ब्रह्म तथा वैयक्तिक आत्माओं अर्थात् जीवों के बीच है।
आत्मा का विकास तथा उसकी आत्यन्तिक मुक्ति
सांसारिकता में लिप्त रहने के कारण जीवात्मा का ज्ञान संकुचित हो जाता है। वह अपने पूर्व-कर्मानुसार शरीर ग्रहण करता और चरम मोक्ष की सम्प्राप्ति तक जन्म-मरण के दुष्चक्र में आबद्ध रहता है। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात् उसका ज्ञान व्यापक हो जाता है। इस स्थिति में उसे पूर्ण ज्ञान हो चुका होता है। रामानुज के उपदेशानुसार आत्मा के गहनतम स्तर को संकुचित करने वाला प्रत्येक कर्म अशुभ एवं इसे व्यापकता प्रदान करने वाला प्रत्येक कर्म शुभ होता है। जब तक जीव को नारायण की कृपा से आत्यन्तिक मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक वह अपने शुभ-अशुभ कामों के माध्यम से स्वयं को व्यापक तथा संकुचित करते हुए इस संसार में विचरण किया करता है। ईश्वरीय कृपा का अवतरण उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो इसके लिए, प्रयत्नशील तथा विशुद्ध होते हैं।
मोक्ष अर्थात वैकुण्ठारोहण
रामानुज के मतानुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा का ऐहिक जीवन के विक्षोभ से मुक्त हो कर एक ऐसे स्वर्ग (वैकुण्ठ) में पहुँच जाना है जहाँ वह ईश्वर के सानिध्य में स्वयं को अप्रतिबन्धित वैयक्तिक परमानन्द में सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित कर लेता है। मुक्तात्मा ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त करता है; किन्तु उसके साथ वह तद्रूपता को प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की सेवा या उपासना में संलग्न हो कर वह उसकी सन्निधि में रहता है। उसके व्यक्तित्व का तिरोभाव नहीं होता। रामानुज के अनुसार जीवन्मुक्ति जैसी कोई बस्तु नहीं है। देह-त्याग के पश्चात् ही मोक्ष-लाभ होता है।
मुक्ति का साधन भक्ति
आत्यन्तिक मुक्ति की सम्प्राप्ति भक्ति एवं भगवत्कृपा द्वारा तथा भगवत्कृपा की सम्प्राप्ति प्रपत्ति अर्थात् पूर्ण आत्म-समर्पण द्वारा होती है। कर्म तथा ज्ञान भक्ति के साधन मात्र हैं।
श्री मध्वाचार्य का द्वैत-दर्शन
प्रस्तावना
श्री मध्वाचार्य ने प्रस्थानत्रय अर्थात् उपनिषद्, भगवद्गीता एवं ब्रह्मसूत्र के आधार पर द्वैत-दर्शन को विकसित किया। यह अविशिष्ट-द्वैतवाद है। रामानुज के वैष्णव-मत से इसके भेद-प्रदर्शन के लिए इसे सद्-वैष्णव-मत की संज्ञा प्रदान की गयी है।
मध्व ईश्वर एवं चेतन तथा अचेतन पदार्थों के बीच आत्यन्तिक भेद के समर्थक है। ईश्वर एकमात्र स्वतन्त्र सत्ता है, जब कि जड़ तथा चेतन पदार्थ पराश्रित सत्ताएँ हैं। माध्व-वेदान्त आत्यन्तिक भेदों का सिद्धान्त है। इसे 'अत्यन्त भेद-दर्शन' कहते हैं। वे निम्नांकित पाँच भेदों (पंच-भेद) पर बल देते हैं :
१. ईश्वर का जीव से भेद।
२. ईश्वर का पदार्थ से भेद।
३. जीव का पदार्थ से भेद।
४. जीव का अन्य जीव से भेद।
५. एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ से भेद।
मध्व का दर्शन भेद का दर्शन है। इस पंच-भेद के प्रति मध्व-प्रतिपादित मत के अनुयायियों की सुदृढ़ आस्था अनिवार्य है।
मध्व ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों तथा भगवद्गीता पर भाष्य लिखे हैं। उपनिषदों के मध्वकृत भाष्य को 'अणुव्याख्यान' कहते हैं। इन भाष्यों के अतिरिक्त इन्होंने महाभारत तथा भागवतपुराण पर संक्षिप्त टीकाएँ भी लिखी हैं। महाभारत पर लिखी इनकी संक्षिप्त टीका को 'भारत-तात्पर्य-निर्णय' कहते हैं। इन भाष्यों तथा संक्षिप्त टीकाओं के अध्ययन से मध्वाचार्य के दर्शन को स्पष्ट रूप से हृदयंगम किया जा सकता है।
मध्व तथा रामानुज के बीच कई-एक दार्शनिक स्थापनाएँ उभयनिष्ठ हैं। मध्व की दार्शनिक मान्यता के अनुसार हरि अर्थात् विष्णु सर्वोपरि सत्ता, जगत् यथार्थ तथा भेद सत्य हैं। सभी जीव भगवान् हरि के आश्रित हैं। वैयक्तिक आत्माओं में ऊर्ध्ववर्तिता तथा अधोवर्तिता के अनुसार कई श्रेणियाँ हैं। जीवात्मा की सहज आनन्दानुभूति ही मुक्ति है। इसी को मोक्ष अथवा चरम मुक्ति कहते हैं। निर्दोष भक्ति मोक्ष-प्राप्ति का साधन है। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द-ये तीन प्रमाण अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति के साधन हैं। हरि का ज्ञान वेदाध्ययन से ही सम्भव है। भागवतपुराण में वर्णित कृष्णोपासना उनके धर्म का केन्द्रस्थ मन्तव्य है और यही है मध्वाचार्य के उपदेशों का सार-तत्त्व।
श्रेणियाँ
माध्वमतानुसार स्वतन्त्र तथा परतन्त्र, पदार्थ अर्थात् वस्तुगत सत्ता के ये द्विविध रूप हैं। ईश्वर एकमात्र सर्वोपरि सत्ता तथा अप्रतिबन्धित यथार्थ है। जीव तथा जगत् उसके ऊपर आश्रित सत्ताएँ हैं। ईश्वर इनका नियम करता है। विधेयात्मक तथा निषेधात्मक-परतन्त्र सत्ताओं के ये दो भेद हैं। चेतन जीवात्माएँ एवं पदार्थ तथा काल की भाँति अचेतन सत्ताएँ, विधेयात्मक सत्ता के ये दो प्रकार हैं। अचेतन तत्त्व वेदों की भाँति नित्य या प्रकृति, काल तथा देश की भाँति नित्यानित्य या प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों की भाँति अनित्य हैं।
परम सत्ता तथा उसकी पार्श्ववर्तिनी
विष्णु अथवा नारायण परम सत्ता है। वह प्रथम वैयक्तिक कारण है। वह विश्व को ज्ञान-सम्पन्न नियन्ता है। वह अपनी पार्श्ववर्तिनी लक्ष्मी के साथ वैकुण्ठ में बाल करता है। ये दोनों सत्य हैं। ब्रह्मा तथा वायु इसके दो पुत्र हैं। वेदाध्ययन से उबाक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। वह स्वयं को अनेकविध व्यूहों तथा अवतारों के मायके हे अभिव्यक्त करता है। पावन प्रतिमाओं में वही विद्यमान है। वह सभी जीवात्माओं श्री अन्तर्निहित नियन्ता अर्थात् अन्तर्यामी है। वह विश्व का स्रष्टा, पोषक एवं संहारक है।
ईश्वर निरवद्य अर्थात् सर्वदोष-रहित है। वह समस्त मांगलिक गुणों से सम्पन्न है। वह सर्वव्यापी और परम स्वतन्त्र है। वह कालातीत तथा देशातीत है। वह लक्ष्मी से महान है; किन्तु अन्य कोई लक्ष्मी से महान् नहीं है। अधीनस्थों या आश्रितों में वह सर्वोपरी है। लक्ष्मी विष्णु भगवान् की शक्ति है। वह उसकी सृजनात्मक शक्ति का मूर्त रूप है। अनेक शरीर-धारण के लिए, उसे किसी प्राकृत शरीर की अपेक्षा नहीं है। विष्णु भगवान की भाँति वह नित्य और सर्वव्यापी है। वह अनन्त काल से अपने स्वामी की महिमा का दर्शन करती आ रही है। वह नित्य-मुक्त, विशोक एवं मेधावी है।
प्रकृति : विश्व का उपादान कारण
ईश्वर जगत् का उपादान कारण न हो कर इसका निमित्त कारण है। इसका कारण यह है कि वह विश्व के आदिम जड़-तत्त्व प्रकृति से भिन्न है। दृश्यमान जगत् के का में परिवर्तित हो जाने वाली यही प्रकृति जगत् का उपादान कारण है। सभी जागतिक पदार्थ, शरीर तथा जीवात्माओं के संघटक-तत्त्व प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। ईश्वर लक्ष्मी के माध्यम से प्रकृति को शक्ति प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप जगत् की सृष्टि होती है।
प्रकृति के पक्ष-त्रय का नियमन तीन शक्तियों-लक्ष्मी, भू तथा दुर्गा द्वारा होता है। अविद्या प्रकृति का ही एक रूप है जो जीव की आध्यात्मिक शक्तियों को आवृत का देती है। यह एक ऐसे आवरण की सृष्टि करती है जिससे सर्वोपरि सत्ता जीव की दृई से ओझल हो जाती है।
महत्, अहंकार, बुद्धि, मन, दश इन्द्रियाँ, पाँच इन्द्रियों के विषय और पंच-महाभूत प्रकृति के ही परिवर्तित रूप हैं जो अपने विकास के पूर्व आद्य मूलभूत प्रकृत के अन्तर्गत सूक्ष्म रूपों में विद्यमान रहते हैं।
जगत् : ईश्वर से भिन्न एक यथार्थ सत्ता
मध्व के मतानुसार जगत् भ्रान्ति नहीं है। दूध से दही की भाँति यह ईश्वर का रूपान्तरण भी नहीं है। वे इसे ईश्वर का शरीर भी नहीं मानते। ईश्वर तथा विश्व का पारस्परिक भेद निरपेक्ष एवं निर्विशेष है। अतः मध्व की दार्शनिक मान्यता को द्वैत कहा जाता है।
जीवात्मा : एक पृथक् सत्ता
जीव अनेक हैं। ये सभी अणु आकार के हैं। समस्त विश्व जीवों अर्थात् वैयक्तिक आत्माओं से परिपूर्ण है। देश का प्रत्येक अणु जीवों से व्याप्त है। मध्व 'तत्त्व-निर्णय' नामक अपने ग्रन्थ में कहते हैं- "देश के एक अणु में निवास करने वाली अनन्त आत्माएँ हैं।"
किन्हीं भी दो जीवों में स्वभावगत सादृश्य नहीं है। वे एक-दूसरे से तत्त्वतः भिन्न हैं। मोक्ष-प्राप्ति के उपरान्त स्वर्ग-सुखोपभोग की स्थिति में भी उनका स्तरगत वैभिन्य बना रहता है।
जीव और ब्रह्म का तात्त्विक भेद
जीव ईश्वर तथा प्रकृति दोनों से भिन्न है। मध्व ब्रह्म और जीव के मध्यगत भेद को यथार्थ मानते हैं।
आकार में परिमित होने पर भी वह अपने ज्ञान-रूप गुण के कारण शरीर में व्याप्त रहता है। जीव सक्रिय कर्ता है; किन्तु वे ईश्वरीय निर्देश पर आश्रित हैं। उनके पूर्व-कर्मानुसार ईश्वर उन्हें कर्म के लिए प्रेरित करता है। वे नित्य और आनन्दस्वरूप हैं; किन्तु पूर्व-कर्मानुसार प्राकृत शरीरों से सम्बद्ध होने के कारण उन्हें दुःख तथा आवागमन के दुष्चक्र में आबद्ध होना पड़ता है। जब तक कश्मलों से उनकी मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वे संसार में भटकते रहते हैं और जन्म-मरण की अन्तहीन आवृत्ति ही उनकी नियति हो जाती है। कश्मलों से मुक्त होने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और तब आत्मा का स्वभावगत आनन्द अभिव्यक्त हो उठता है।
मोक्ष से आत्मा ईश्वर के समकक्ष नहीं हो जाता
आत्मा ईश्वर के समान नहीं हो जाता। वह केवल उसकी सेवा का अधिकारी है।
स्वर्ग में जीवों में तात्त्विक भेद होते हैं। उस आनन्द-लोक में भी जीवों के विभिन्न वर्ग तथा स्तर हैं। मुक्तात्मा परस्पर समकक्ष नहीं होते; किन्तु उनमें पारस्परिक विसंगति भी नहीं है, क्योंकि ये सभी ब्रह्मज्ञानी और निरवद्य हैं।
आत्माओं का वर्गीकरण
मध्व को रामानुज द्वारा प्रतिपादित आत्माओं का त्रिवर्गीय विभाजन मान्य है। ये तीन वर्ग हैं-नित्य (यथा लक्ष्मी), मुक्त (यथा देव, मनुज, ऋषि, सन्त तथा पितृगण) और बद्ध। तृतीय वर्ग (बद्ध) के दो भेद हैं। पहले वर्ग में वे लोग आते हैं जो मुक्ति-योग्य हैं और दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो मुक्ति के योग्य नहीं हैं। जिन लोगों हे मुक्ति की योग्यता नहीं है, उन्हें पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में वे लोग आते हैं जो संसार-चक्र में अनन्त काल के लिए आबद्ध (नित्य-संसारिणः) हो चुके रहते हैं और घोर तमिस्रा का अन्धकूप ही जिनकी नियति है, वे दूसरे वर्ग में आते हैं।
कुछ आत्माओं का मोक्ष उनकी अन्तर्निहित योग्यता के अनुरूप पूर्व-निर्धारित होता है और कुछ अन्य जीव ऐसे होते हैं जिनके भाग्य-पटल पर संसार का अन्तहीन परिभ्रमण या तमोमय लोक में प्रवेश लिपिबद्ध हो चुका होता है। सात्विक आत्माओं को स्वर्ग प्राप्त होता है, राजसिक आत्मा संसार में चक्रवत् भ्रमण करता है और मोगुणी आत्मा नरक में गिरता है।
भक्ति : मुक्ति का साधन
भक्ति मुक्ति का साधन है। जीव को ईश्वरानुग्रह से मुक्ति प्राप्त होती है। भक्त इस ईश्वरानुग्रह को विष्णु-पुत्र वायु के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। ईश्वर तक पहुँच पाने का कोई सुस्पष्ट मार्ग नहीं है। उसकी प्राप्ति वायु की मध्यस्थता से ही सम्भव है। भक्ति की तीव्रता के अनुपात से ही ईश्वर-कृपा की सम्प्राप्ति होती है।
ईश्वरोपासना भगवत्कृपा की प्राप्ति की अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता है। जीवात्मा की सुरक्षा उसके इस बोध पर निर्भर है कि वह ईश्वर पर आश्रित तथा उसके नियन्त्रण में है। सम्यक् ज्ञान की परिसमाप्ति ईश्वरीय प्रेम में होती है। भक्ति ईश्वर की महिमा के ज्ञान का परिणाम है।
अंकन, नामकरण, भजन तथा स्मरण
शरीर पर भगवान् विष्णु के प्रतीकों का अंकन, उनके नाम पर पुत्र-पौत्रादि का नामकरण, उनकी महिमा का गायन और उनके अविकल स्मरण का अभ्यास उनकी उपासना के अंग हैं। मध्य कहते हैं- "ईश्वर के स्मरण के दृढ़ अभ्यास से ही मृत्यु के समय तुम्हें उनका अनायास स्मरण हो जायेगा।" वे इस तथ्य के प्रति संकेत करते हैं कि अवतार-ग्रहण के समय ईश्वर ने कोई प्राकृत शरीर नहीं धारण किया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को उपवास-व्रत के कठोरतापूर्वक पालन का निर्देश दिया था।
साधना का अभ्यास
मोक्ष-प्राप्ति के लिए निर्मल नैतिक जीवन प्रारम्भिक आवश्यकता है। यदि साधक ईश्वर-साक्षात्कार का इच्छुक है, तो उसे वेदाध्ययन, इन्द्रिय-निग्रह, अनासक्ति तथा पूर्ण आत्म-समर्पण की भावना से सुसम्पन्न रहना चाहिए। त्याग, भक्ति तथा ईश्वर के ध्यान-जनित ज्ञान द्वारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ध्यान तथा दैवी कृपा से भक्त को ईश्वर की प्रत्यक्ष सहजानुभूति होती है और वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।
द्वैतवाद-दर्शन के प्रख्यात व्याख्याता श्री मध्वाचार्य की ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएँ हैं।
श्री निम्बार्क का द्वैताद्वैत-दर्शन
प्रस्तावना
निम्बार्काचार्य द्वारा प्रतिपादित यह दर्शन भेदाभेद-दर्शन के नाम से भी प्रख्यात है। इसे उन्होंने ही पल्लवित-पुष्पित किया। निम्बार्क वैष्णव-मतावलम्बी तेलुगु ब्राह्मण थे। इनका जीवन-काल मध्व के पूर्व तथा रामानुज के पश्चात् ग्यारहवीं शताब्दी का माना जाता है। कहा जाता है कि वे सूर्य के अवतार थे।
उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर 'वेदान्त-सौरभपारिजात' नामक एक संक्षिप्त भाष्य तथा 'दशश्लोकी' नामक ग्रन्थ की रचना की। अपने भाष्य में उन्होंने ब्रह्मपरिणामवाद नामक सिद्धान्त को विकसित किया।
निम्बार्क का मत भास्कर के विचारों से अत्यधिक प्रभावित है। भास्कर का जीवन-काल नौवीं शताब्दी के पूर्वार्ध का है। इन्होंने वेदान्त-दर्शन की व्याख्या ऐताद्वैत-मत के आधार पर की है। यह सिद्धान्त भास्कर की कोई मौलिक खोज नहीं थी। इसकी परिपुष्टि व्यास-रचित ब्रह्मसूत्र में उल्लेखित प्राचीन आचार्य औडुलोमि द्वारा इसके पूर्व ही की जा चुकी थी ।
ईश्वर, आत्मा तथा जगत् भेद में अभेद
निम्बार्क के मतानुसार ईश्वर का जीव तथा जगत् से भेदाभेद-सम्बन्ध है। जीव और जगत् ईश्वर से भिन्न हैं, क्योंकि उनमें जो गुण हैं, वे उन गुणों से भित्र हैं जो ईश्वर में है, किन्तु इसके साथ ही ये परस्पर भिन्न भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है और ये उस पर आश्रित हैं।
निम्बार्क का दर्शन ब्रह्म को परम सत्ता मानता है जो अद्वितीय है। जीव और जगत् उसकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्तियाँ हैं।
जीव तथा ब्रह्म आत्मचेतन हैं। किन्तु जीव परिच्छिन्न और ईश्वर अपरिच्छिन्न है। ईश्वर स्वतन्त्र सत्ता है। जीव तथा प्रकृति की सत्ता परतन्त्र है। जीव भोक्ता, जगत् भोग्य और ब्रह्म सर्वोपरि नियन्ता है।
जीव और जगत् ईश्वर से नितान्त भिन्न नहीं हैं। यदि परम सत्ता वैयक्तिक आत्मा तथा जगत् से नितान्त भिन्न हो, तो वह सर्वव्यापी नहीं हो सकती। इस स्थिति में वह वैयक्तिक आत्मा और जगत् की भाँति ही परिच्छिन्न हो जायेगी और तब उसे उनके नियंता की संज्ञा नहीं प्रदान की जा सकेगी। निम्बार्क के मतानुसार भेद तथा अभेद, होनी सत्य हैं। जीव और जगत् ब्रह्म से इसलिए भिन्न हैं कि इनके गुण तथा स्वरूप ब्रह्म के गुण तथा स्वरूप से भिन्न हैं; किन्तु इसके साथ ही वे उससे अभिन्न भी हैं, क्योंकि वे स्वयं-स्थित न हो कर पूर्णतः ब्रह्म पर आश्रित हैं। इस प्रकार का सम्बन्ध सूर्य तथा उसकी किरणों और अग्नि तथा उसके स्फुल्लिंगों में पाया जाता है। जीव और जगत् ईश्वर से भिन्न हैं; किन्तु उनमें वैसा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है जैसा लहरों का जल से और एस्सी का उसकी गाँठों से होता है। ये दोनों ब्रह्म से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी।
परम सत्ता तथा उसके लक्षण
इस मत के अनुसार ब्रह्म जगत् का निमित्त तथा उपादान, दोनों कारण है। वह निर्गुण भी है और सगुण भी; क्योंकि वह सृष्टि में निःशेष न हो कर इसका अतिक्रमण भी कर जाता है।
परम सत्ता के चार रूप
परम सत्ता चार रूपों में विद्यमान है। अपने आद्य रूप में वह अप्रतिबन्धित तथा निर्विकार परम ब्रह्म है और अपने द्वितीय रूप में विश्व का अधिपति ईश्वर है। तृतीय रूप में उसे जीव अथवा वैयक्तिक आत्मा के नाम से अभिहित किया जाता है और चतुर्थ रूप में वह स्वयं को नामरूपात्मक जगत् के रूप में अभिव्यक्त करता है। दृश्यमान जगत् ब्रह्म का एक अंश है। इसका ब्रह्म से कोई पृथक् और स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। विश्व और ब्रह्म के बीच भेदाभेद-सम्बन्ध है। जगत् ब्रह्म से भिन्न नहीं है।
कृष्ण-सर्वोपरि सत्ता
परम सत्ता समस्त दोषों से रहित है। दिव्य देहधारी इस सत्ता में समस्त मांगलिक गुण विद्यमान हैं। वह सौन्दर्य, प्रेम, माधुर्य तथा लालित्य से ओत-प्रोत है।
निम्बार्क परम ब्रह्म तथा कृष्ण को अभिन्न मानते हैं। वह समस्त मांगलिक गुणों से सम्पन्न और अहम्मन्यता, अज्ञान, वासना तथा आसक्ति से मुक्त है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध उसके चार स्वरूप (व्यूह) हैं। वह स्वयं को अवतारों के रूप में प्रकट किया करता है। निम्बार्क के मतानुसार कृष्ण तथा राधा नारायण तथा लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राधा गोपियों में प्रमुख होने के साथ-साथ भगवान् कृष्ण की पार्श्ववर्तिनी अथवा शक्ति भी हैं।
ब्रह्म जगत् का उपादान एवं निमित्त कारण किस प्रकार है
ब्रह्म जगत् का उपादान एवं निमित्त कारण है। उसकी सूक्ष्मरूपिणी चित्- अचित् शक्तियाँ स्वयं को सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त करती हैं; अतः वह उपादान कारण है। पुनः वह जीवात्माओं को उनके कर्मों तथा फलों के साथ संयुक्त करता तथा अनुभव-प्राप्ति के लिए उनके लिए समुचित साधनों की व्यवस्था करता है; अतः वह निमित्त कारण है।
ब्रह्म को सृष्टि-रचना के लिए किसी बाह्य सामग्री, साधनों और उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। उसे हाथों या अन्य किन्हीं उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं होती। वह सर्वशक्तिमान् तथा अपने संकल्प मात्र से सृष्टि-रचना में समर्थ है। उसका सत्-संकल्प ही जगत् के रूप में परिणत हो जाता है। जिस प्रकार कोई मकड़ा अपने शरीरस्थ तन्तुओं से जाला बुन लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म ने स्वयं से ही सृष्टि की रचना की है। उपनिषदों की यही उद्घोषणा है। इस प्रकार सृष्टि की संरचना में ब्रह्म उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। सर्वशक्तिमान् होने के कारण वह परिणमन एवं उसके साथ ही स्वयं को इससे असम्पृक्त या परे रहने देना पूर्णत: उसकी शक्ति में है । यह तथ्य उपनिषदों तथा ब्रह्मसूत्र द्वारा भी समर्थित है । ब्रह्म ने अपने तात्विक स्वरूप को प्रभावित रखते हुए स्वयं को जगत के रूप में परिणत किया है । ब्रह्म के स्वरूप से अर्न्भूत रहस्यमयी सृजनात्मक शक्ति ही इसका कारण है ।
व्यष्ट आत्मा और समष्टि आत्मा का पारस्परिक सम्वन्ध उ
पाधिगत भेद तथा तात्त्विक एकरूपता
वैयक्तिक आत्या परम सत्ता का एक अंश है; किन्तु वह परमात्मा से अभिन्न भी है । जिस प्रकार एक तरंग समुद्र का एक अंश होने के कारण उससे भिन्न और दोनों के जल होने के कारण उससे अभिन्न है, उसी प्रकार वैयक्तिक आत्मा परमात्मा का एक होने के कारण उससे भिन्न और दोनों के चिन्मय-स्वरूप होने के कारण उससे अभिन्न भी है। वैयक्तिक आत्मा अर्थात् जीव तथा परमात्मा अर्थात् ब्रहा के पारस्परिक में उपाधिगत भेद और तात्विक तादात्म्य, दोनों अन्तर्निहित हैं। जीव और हा भेद स्वरूपगत न हो कर मात्रागत है। प्रतिभासिकता के सन्दर्भ में जीव ब्रह्म से किन्तु तत्वतः वह उससे अभिन्न तथा अविभाज्य है। इसी को भेदाभेद कहा गया है ।
प्रबल वायु के द्वारा समुद्र के उद्वेलित होने पर तरंग उठने लगती है। तरंग समुद्र एक अंश होने पर भी उससे भिन्न है। किन्तु वायु के शान्त होने पर तरंग भी शान्त होकर समुद्र से अभिन्न हो जाती है। इसी प्रकार एषणाओं से विक्षुब्ध मन इन्द्रियों-सहित विषयोन्मुखी हो कर स्वयं में एक भिन्न व्यक्तित्व का आरोपण कर बैठता है। इस अहंभाव-ग्रस्त परिच्छिन्न जीव को प्रपंचात्मक जगत् के सम्पर्क के अनेकविध अनुभव प्राप्त होते हैं; किन्तु एषणाओं के उन्मूलन के पश्चात् जब पूर्णतः शान्त हो जाता है, तब उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं रह जाता और उसकी समस्त वृत्तियों का उपशमन हो जाता है। इस स्थिति में प्रातिभासिक जगत् का निषेध हो जाता है और परिच्छिन्न आत्मा अपरिच्छिन्न आत्मा अर्थात् ब्रह्म का कार कर लेती है।
जीव तथा उसके गुण
आत्माएँ, असंख्य तथा अणु आकार की हैं। जीव आणविक एवं ज्ञानस्वरूप है। जीव के प्रति यह अवधारणा शंकर की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। जिस पूर्व प्रकाश तथा प्रकाश का स्रोत-दोनों है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञाता भी। आत्मा का अपने गुणों के साथ धर्मी-धर्म-सम्बन्ध है। इसे भेदाभेद-सम्बन्ध कहते हैं।
अणु आकार का होते हुए भी जीव अपने ज्ञान के सर्वव्यापी गुणों के कारण दैहिक सुख-दुःख का अनुभव करता है। वह नित्य है। सुषुप्ति तथा मुक्ति की उच्चतम अवस्था में भी इसका अस्तित्व अक्षुण्ण रहता है। प्रलय काल में जगत् तथा वैयक्तिक आत्माएँ सूक्ष्म रूप में ईश्वर में विलीन हो जाती हैं। जन्म-मरण का सम्बन्ध केवल शरीर से है। आत्मा इससे अप्रभावित रहती है।
वैयक्तिक आत्मा कर्ता है। इसमें न तो स्वतन्त्र ज्ञान है, न स्वतन्त्र कर्तृत्व। वैयक्तिक आत्माएँ तथा जगत् आत्म-निर्भर नहीं हैं। इनका मार्गदर्शन, धारण तथा नियमन ईश्वर द्वारा होता है। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म के व्यष्टिगत स्वरूप की एक किरण है। वैयक्तिक आत्मा प्रत्येक अवस्था में आनन्द से सम्बद्ध रहती है।
जीवों की श्रेणियाँ
जीवों की दो श्रेणियाँ हैं। जिनको सर्वव्यापी अन्तरात्मा अर्थात् परमात्मा का ज्ञान एवं दृश्यमान जागतिक प्रपंच तथा ब्रह्म की अभिन्नता का सर्वतोभावेन बोध हो चुका है, वे प्रथम श्रेणी में आते हैं। उनको मुक्तात्मा कहा जाता है। वे अज्ञान-रहित होते हैं। किन्तु जो केवल इस दृश्यमान जगत् को ही देख पाते हैं और जिन्हें नामरूपात्मक जगत् के अधिष्ठान सर्वव्यापी अन्तरात्मा अर्थात् परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उनकी गणना द्वितीय श्रेणी में की जाती है। इन्हें बद्ध जीव कहा जाता है।
जगत् : ब्रह्म की यथार्थ अभिव्यक्ति
निम्बार्क के अनुसार जगत् एक भ्रान्त प्रतीति नहीं है। यह ईश्वर में अधिष्ठित सूक्ष्म-रूपिणी शक्ति का परिणाम है।
जगत् असत् या भ्रान्ति न हो कर ब्रह्म की एक यथार्थ अभिव्यक्ति या इसका परिणाम है। उसे केवल इसी अर्थ में असत् कहा जा सकता है कि वह अस्तित्व की वर्तमान स्थिति में 'स्वतन्त्र सत्ता-भाव' से शून्य है और ब्रह्म से विलग उसका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार जल से तरंग या बुलबुला भिन्न तथा अभिन्न-दोनों है, उसी प्रकार जगत् भी ब्रह्म से भिन्नाभिन्न है।
मुख्य तत्त्वों की संख्या तीन है : (१) अप्रकृति-इसका आविर्भाव आद्य प्रकृति से नहीं हुआ है। यह ईश्वर के दिव्य शरीर का उपादान (रामानुज के शब्दों में शुद्ध सत्त्व) तथा उसकी नित्य विभूति की आधार-भित्ति है। (२) त्रिगुणात्मक प्रकृति-सत्व, रजस् एवं तमस् से समन्वित यह त्रिगुणात्मक तत्त्व है। (३) काल। ये तीन तत्त्व भी जीवात्माओं की भाँति नित्य हैं।
निम्बार्क के अनुसार ब्रह्म की शक्ति जगत् का उपादान कारण है। शक्तिगत परिवर्तन से ब्रह्म की अखण्डता प्रभावित नहीं होती। रामानुज जिसे 'ब्रह्म का शरीर' कहते हैं, उसे निम्बार्क ने 'शक्ति' के नाम से अभिहित किया है।
मोक्ष
अविद्या अनादि है। कर्म अविद्या का परिणाम है जिससे जीव की शुचिता आवृत हो जाती है। ईश्वर की कृपा से अविद्या की निवृत्ति सम्भव है।
शुद्ध भक्ति तथा यथार्थ ज्ञान मोक्ष के साधन
प्रपत्ति अर्थात् ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण मोक्ष का साधन है। जो प्रपन्न है, उस पर ईश्वर की कृपा-वृष्टि होती है। इस कृपा-वृष्टि के कारण भक्त अपन अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म-साक्षात्कार में समर्थ हो जाते हैं। ईश्वर उनके भीतर भक्ति का सबार करता है जो ईश्वर-साक्षात्कार में परिणत हो जाती है।
भक्ति के अन्तर्गत ब्रह्म का ज्ञान, जीवात्मा का स्वरूप तथा ईश्वर-कृपा का सुफल अर्थात् मुक्ति-ये सभी सन्निहित हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आत्मा से शरीर, इन्दिय-समुदाय तथा मन के तादात्म्य की भ्रान्त अवधारणा जैसे प्रतिबन्धकों के स्वरूप का भी समावेश है जो ईश्वर-साक्षात्कार में बाधक हैं।
मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति से होती है। यथार्थ ज्ञान से ब्रह्म का सत्य-स्वरूप अनावृत हो जाता है और शुद्ध भक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण के लिए प्रेरित करती है। दिव्य भोगों के समय जीव अपनी वैयक्तिक सत्ता को अक्षुण्ण रखने में समर्थ है। किन्तु उसकी इच्छा ब्रह्म के संकल्प की वशवर्तिनी है। मोक्ष के समय भी जीव की वैयक्तिकता का तिरोभाव नहीं होता। वह इस स्थिति में भी ब्रह्म से भिन्न भी है और अभिन्न भी। इसी को भेद में अभेद अर्थात् भेदाभेद कहते हैं।
मोक्ष : परमात्मा से एकत्व-बोध की एक स्थिति
ब्रह्म मुक्तात्माओं के समक्ष स्वयं को अपने महिमा-मण्डित आद्य स्वरूप में उलट करता है; किन्तु ऐसा वह किसी देव-विशेष के रूप में नहीं करता। जीव को इस सत्य का बोध हो जाता है कि वह ब्रह्म का एक अविभाज्य अंग है। अपनी वृद्धावस्था में से अपने पृथक् अस्तित्व का जो भान हुआ करता था, वह अब नष्ट हो जाता है।
वह अपने पूर्व-बन्धनों से मुक्त हो कर अपने सत्य-स्वरूप अर्थात् ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब उसे ब्रह्म के साथ अपने एकत्व का बोध हो चुका है। अब संसार में उसका पुनरागमन नहीं होगा; क्योंकि वह जन्म-मरण के चक्र से एक हो चुका है। ब्रह्म से एकात्मकता के कारण अब उसे उसकी समकक्षता की प्राप्ति हो चुकी है; किन्तु वह सृष्टि की रचना, उसके पालन तथा उसके संहार की शक्ति से वंचित है।
श्री वल्लभ का शुद्धाद्वैत-दर्शन
प्रस्तावना
वल्लभ को शंकर द्वारा प्रतिपादित माया का सिद्धान्त मान्य नहीं है। उनके मतानुसार यह जड़-चेतन जगत् सत्य और ईश्वर का ही सूक्ष्म रूप है। यही कारण है कि उनके दार्शनिक सिद्धान्त को शुद्धाद्वैत कहा जाता है। जो लोग जगत् की व्याख्या माया के माध्यम से करते हैं, वे विशुद्ध अर्थों में वेदान्ती नहीं हैं; क्योंकि वे ब्रह्म के अतिरिक्त एक अन्य सत्ता को भी स्वीकार कर लेते हैं। वल्लभ के मान्यतानुसार ब्रह्म माया जैसे तत्त्वों से असम्बद्ध रह कर भी सृष्टि-रचना में समर्थ है; किन्तु शंकर माया की शक्ति को विश्व तथा ब्रह्म के बीच एक संयोजक तत्त्व के रूप में रेखांकित करते हैं। अतः वल्लभ के दार्शनिक सिद्धान्त को शुद्धाद्वैत कहा जाता है। वल्लभ ने ब्रह्मसूत्रों पर स्व-रचित अपने 'अणुभाष्य' में अपनी इस दार्शनिक प्रणाली का प्रतिपादन किया है। शंकर के केवलाद्वैत तथा रामानुज के विशिष्टाद्वैत के विपरीत उन्होंने अपने मत को शुद्धाद्वैत के नाम से अभिहित किया। वल्लभ दक्षिण भारत के तेलुगु ब्राह्मण थे। उन्होंने उत्तर भारत में आ कर विष्णु स्वामी के दार्शनिक मत को विकसित किया। विष्णु स्वामी का जीवन-काल तेरहवीं शताब्दी था। उनके मत को ब्रह्मवाद कहते हैं।
वल्लभ का कहना है कि समस्त जगत् यथार्थ तथा सूक्ष्म रूप से ब्रह्म है। वैयक्तिक आत्माएँ तथा जड़ जगत् तात्त्विक रूप से ब्रह्म से अभिन्न हैं। जीव, काल तथा प्रकृति अथवा माया नित्य तत्त्व हैं; किन्तु ब्रह्म से अलग उनकी कोई पृथक् सत्ता नहीं है।
वल्लभ संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। सर्वप्रथम वे मथुरा में आये और तत्पश्चात् वाराणसी में। उन्होंने वैष्णव-मत तथा दर्शन का प्रचार अत्यन्त लगन तथा उत्साह के साथ किया। उन्होंने राजस्थान तथा गुजरात में वैष्णव-मठों की स्थापना की। नाथद्वारा में उनके बहुसंख्यक अनुयायी पाये जाते हैं।
वल्लभ की प्रमुख रचनाऍं
वल्लभ केवल उपनिषदों, भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्रों को ही नहीं; अपितु भागवतपुराण की प्रामाणिकता को भी स्वीकार करते हैं। 'व्याससूत्रभाष्य (अणुभाष्य), 'जैमिनिसूत्रभास्य', 'भागवत-टीका-सुबोधिनी', 'पुष्टिप्रवाहमर्यादा' तथा 'सिद्धान्तरहस्य' उनके प्रमुख ग्रन्थ हैं। उन्होंने व्रजभाषा में भी कई ग्रन्थों की रचना की है। उनके मतानुसार शास्त्र ही अन्तिम प्रमाण हैं।
उपासना तथा भगवत्कृपा पर बल
वल्लभ के मत में कृष्ण के रूप में विष्णु की उपासना ही धर्म है। चैतन्य की उपासना-पद्धति के उद्भव का स्रोत भी मुख्यतः रामानुज द्वारा प्रतिपादित वैष्णव-दर्शन ही है। यह सच्चिदानन्द ईश्वर के सगुण एवं हितकारी स्वरूप की अवधारणा पर केन्द्रित है। भगवान् कृष्ण सर्वोच्च ब्रह्म हैं। उनका विग्रह सत्-चित्-आनन्द से युक्त है। उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है।
वल्लभ के अनुयायी बाल-कृष्ण की उपासना करते हैं। उनके प्रति उनमें वात्सल्य-भाव रहता है। वल्लभ पुष्टि तथा भक्ति पर अत्यधिक बल देते हैं। महापुष्टि ईश्वर की महती कृपा अथवा अनुग्रह है जो भगवत्प्राप्ति में भक्तों के लिए सहायक सिद्ध होती है।
ईश्वर : एकमात्र सत्ता
वल्लभ के अनुसार ईश्वर निरपेक्ष सत्ता अथवा पुरुषोत्तम है। वह पूर्ण तथा सच्चिदानन्द है। वह असीम, नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान् है। वह समस्त मांगलिक गुणों का आगार है। श्रुतियाँ उसे निर्गुण कहती हैं; किन्तु इसका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि उसमें साधारण गुण नहीं हैं।
ईश्वर यथार्थ है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई यथार्थ सत्ता नहीं है। वह एकमात्र यथार्थ सत्ता है। वह जगत् एवं जीवात्माओं का मूल स्रोत है। वह प्रथम एवं एकमात्र कारण है। ईश्वर सृष्टि का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। वह मात्र अपनी इच्छा-शक्ति से सृष्टि की रचना करता है। ब्रह्म स्वेच्छा से स्वयं को जीवात्माओं तथा जगत् के रूप में प्रकट करता है; किन्तु इससे उसके तात्विक स्वरूप में कोई विकार नहीं आता। अग्नि से स्फुलिंगों के स्फुरण की भाँति अक्षर ब्रह्म (सत्-चित्-आनन्द) से जागतिक प्रपंच का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्म स्रष्टा तथा सृष्टि-दोनों है।
ज्ञान तथा कर्म-इन दो गुणों से समन्वित ईश्वर कृष्ण का रूप ग्रहण कर लेता है। अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, वह स्वयं को नानाविध रूपों में प्रकट करता है।
प्राकृत जगत् तथा मिथ्या संसार
जगत् ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यह ब्रह्म का परिणाम तथा उसी के सदृश नित्य तथा सत्य है। जड़ जगत् ब्रह्ममय है। जगत् भ्रान्त प्रतीति नहीं है। तत्त्वतः यह ब्रह्म से अभिन्न है।
जगत् प्राकृत है। यह मायिक न हो कर यथार्थ है। यह ईश्वर का ही समष्टिगत रूप है। किन्तु संसार का यह क्षणस्थायी प्रपंच मायिक है। वैयक्तिक आत्मा अपने चतुर्दिक् व्याप्त 'अहं' तथा 'मम' की अवधारणा से इसकी सृष्टि कर लेती है। अहं-भाव के कारण ईश्वर से वियुक्त जीव को अपना मूल, सत्य तथा दिव्य स्वस्य विस्मृत हो जाता है। संसार जीवात्मा की कल्पना तथा उसके कर्म का परिणाम है जो उसके 'अहं' तथा 'मम' के चतुर्दिक् क्रियाशील रहता है। अपने स्वार्थ के कारण वह जीवात्माओं तथा वस्तुपरक विश्व से भ्रान्तिजन्य सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। वह अपने लिए स्वयं एक जाल बुन कर उसमें उलझ जाता है। यह एक भ्रम है; क्योंकि यह जाल यथार्थ नहीं है। जीव द्वारा रचित मिथ्या सम्बन्धों का यह संसार मात्र माया है। इस संसार अथवा माया के प्रादुर्भाव का कारण यह है कि आत्मा जो ईश्वर से अविभक्त है. स्वयं को एक स्वतन्त्र सत्ता या इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करने लगती है। ईश्वर से वियुक्त आत्मा, इसका शरीर तथा इसका संसार-ये सभी मायिक हैं। इसी को संसार की संज्ञा प्रदान की गयी है। यह प्राकृत जगत् से नितान्त भिन्न है।
जीव तथा ब्रह्म अग्नि तथा स्फुलिंग का दृष्टान्त
जीव ब्रह्म का परिणाम न हो कर उसके अंश हैं। अग्नि के स्फुलिंग की भाँति वे उससे स्वतः प्रादुर्भूत हो जाते हैं। ब्रह्म पूर्ण तथा जीव अंश हैं; किन्तु ब्रह्म तथा जीव अर्थात् वैयक्तिक आत्मा में कोई तात्त्विक भेद नहीं है, क्योंकि दोनों के अन्तर्निहित तत्त्वों में समरूपता है। जीव ब्रह्म से अभिन्न और ब्रह्म के ही सदृश यथार्थ तथा नित्य है।
जीवात्मा अविद्या से आवृत ब्रह्म नहीं है। वह स्वयं ब्रह्म है; किन्तु उसका गुण 'आनन्द' 'आच्छादित' या 'अव्यक्त' है। अचेतन जगत् या जड़ पदार्थ में भी आनन्द आच्छादित या अव्यक्तावस्था में विद्यमान रहता है; किन्तु जब आत्मा को दिव्य आनन्द की तथा जगत् को चेतना तथा दिव्य आनन्द-दोनों की ही सम्प्राप्ति हो जाती है, तब ब्रह्म से इनका भेद समाप्त हो जाता है।
आत्मा कर्ता भी है और भोक्ता भी। यह अणु आकार का है। किन्तु जिस प्रकार चन्दन अपनी सुगन्ध से उस स्थान को भी आप्लावित कर देता है जहाँ वह स्वयं स्थित नहीं रहता या जिस प्रकार किसी कक्ष के एक स्थान-विशेष पर रखा हुआ दीप सम्पूर्ण कक्ष को आलोकित कर देता है, उसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञान-रूप गुण के कारण समग्र शरीर में व्याप्त रहता है।
जीवात्माओं का वर्गीकरण
शुद्ध, संसारी तथा मुक्त-ये जीवात्माओं के तीन प्रकार हैं। शुद्ध जीवात्माओं के ऐश्वर्यादि दिव्य गुण अविद्या के कारण मलिन नहीं होने पाते। संसारी जीव अविद्या या अज्ञान के पाश में आबद्ध रहते हैं। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से सम्बन्ध रहने के कारण उन्हें जन्म-मरण का अनुभव प्राप्त हुआ करता है। मुक्त जीव विद्या या ज्ञान के कारण सांसारिक बन्धनों से मुक्त रहते हैं। जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब उसे अपने अव्यक्त गुण पुनः प्राप्त हो जाते हैं और वह ईश्वर या ब्रह्म के साथ समरूप हो जाता है। जिसे सत्य या ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, उसके लिए समग्र जगत् ब्रह्मवत् हो जाता है।
आत्माओं का वर्गीकरण एक अन्य विधि से भी हुआ है। इस वर्गीकरण के अनुसार पुष्टि, मर्यादा तथा प्रवाहिका-जीवात्माओं के ये तीन प्रकार होते हैं। अपनी उत्पत्ति, प्रकृति तथा अपनी अन्तिम दशा के सन्दर्भ में ये परस्पर भिन्न हैं; किन्तु अपने पारस्परिक वैभिन्य के साथ-साथ ये सभी ईश्वर से ही प्रादुर्भूत होते हैं।
ईश्वर की आनन्द-काया से प्रादुर्भूत होने के कारण पुष्टि जीव सर्वोच्च हैं। वे ईश्वर के अंश होते हैं। ईश्वर अंशी अर्थात् पूर्ण इकाई है। वे भगवत्कृपा प्राप्त जीव हैं। उनमें दैवी बीज अन्तर्निहित रहते हैं जो अन्ततः सुफल प्रदान करते हैं। ईश्वरानुग्रह से उन्हें अन्ततोगत्वा लक्ष्य-प्राप्ति होती है। उन्हें भगवान् कृष्ण के घनिष्ठतम नैकट्य एवं उनके प्रति सख्य-भाव का प्रसाद मिलता है। भगवत्कृपा से उनमें भक्ति का विकास होता है। भक्ति स्वयं में ही साधन तथा साध्य द्विविध-रूपा है।
मर्यादा जीवों का प्रादुर्भाव वाक् अर्थात् ईश्वर-प्रोक्त शब्द से होता है। इनका नियमन भगवत्कृपा से न हो कर विधि-विधान से होता है। सर्वप्रथम इनके कर्मकाण्डीय अनुष्ठान स्वार्थ से उत्प्रेरित होते हैं; किन्तु शनैः-शनैः उनमें निष्काम भाव विकसित होता जाता है और उनके उक्त अनुष्ठान निष्काम भाव से होने लगते हैं। इससे उनकी चित्त-शुद्धि होती है जिसके फलस्वरूप वे उस अक्षर तह पहुँच जाते हैं जो एक प्रकार से ईश्वर के परम धाम का मुख्य द्वार है। इसके पश्चात् उन्हें परम धाम की प्राप्ति हो जाती है।
प्रवाहिका जीवों का प्रादुर्भाव ईश्वर के मन से होता है। वे सांसारिक जीव होते हैं। उनका सम्बन्ध न तो भगवत्कृपा से होता है, न विधि-विधान से। प्रवाह अर्थात् सतत संसरण ही इनकी नियति है।
इस त्रिवर्गीय विभाजन में एक उप-विभाजन भी है जिसके अनुसार जीव समुदाय पुष्टि-पुष्टि, पुष्टि-मर्यादा, पुष्टि-प्रवाहिका, मर्यादा-मर्यादा, मर्यादा-पुष्टि मर्यादा-प्रवाहिका, प्रवाहिका-प्रवाहिका, प्रवाहिका-पुष्टि तथा प्रवाहिका-मर्यादा में विभक्त है।
पुष्टि-मार्ग अथवा भगवत्कृपा का मार्ग
जीवनचर्या एवं मोक्ष के सम्बन्ध में वल्लभ द्वारा उपदिष्ट मार्ग को पुष्टि-मार्ग- कहा जाता है। मनुष्य का अन्त करण पाप से मलिन हो गया है; अतः अपने उन्नयन एवं मोक्ष के लिए उसे भगवत्कृपा की अत्यधिक आवश्यकता है। जीव को भगवतकृपा से पुष्ट तथा पोषण की सम्प्राप्ति होती है; अतः इसे पुष्टि-मार्ग कहा जाता है।
जीव को भगवत्कृपा से ही आत्यन्तिक मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति मोक्ष-प्राप्ति का प्रमुख साधन है। ज्ञान भी उपयोगी है। महापुष्टि प्रतिन्यक विघ्नों के व्याघात तथा ईश्वर-प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। विशेष कृपा से प्रादुर्भूत भक्ति को पुष्टि-भक्ति कहते हैं।
चतुर्विध भक्ति
प्रवाह-पुष्टि-भक्ति, मर्यादा-पुष्टि-भक्ति, पुष्टि-पुष्टि-भक्ति तथा शुद्धा-पुष्टि-भक्ति-पुष्टि-भक्ति के ये चार प्रकार होते हैं। प्रवाह-भक्ति-मार्गी जन सांसारिकता में संलग्न रहते हुए भगवत्प्राप्ति के साधन विहित कर्म करते रहते हैं । सांसारिकता की तुलना सरित-प्रवाह से की गयी है। मर्यादा-भक्ति उन लोगों का मार्ग है जो भगवत्कृपा से उपासना के लिए उपयुक्त ज्ञान की सम्प्राप्ति के अधिकारी हो चुके रहते हैं। वे भागवत विधि-विधान से पूर्णतः अभिज्ञ और ज्ञान-प्राप्ति के लिए स अपने ही प्रयत्नों पर निर्भर रहते हैं। पुष्टि-भक्ति में भक्त जन आत्म-निग्रह का जीवन व्यतीत करते हैं। वे भगवत्कथा का श्रवण, कीर्तन, प्रभु का प्रशस्ति-गायन और मन्त्र जप करते हैं।
शुद्धा-पुष्टि-भक्ति अथवा भक्ति का विशुद्धतम रूप
शुद्धा-पुष्टि-भक्ति-मार्गी भक्त कीर्तन तथा भगवन्नाम का गायन करते हैं। वे ईश्वर का गुणगान करते हैं। इन सबके लिए उनके अन्तर्गत एक प्रबल संवेग का विकास हो चुका रहता है। इस प्रकार की भक्ति स्वयं प्रभु से ही निःसृत होती है। भक्तों पर प्रभु की कृपा-दृष्टि के फलस्वरूप उनमें प्रभु के प्रति प्रेम का स्फुरण होता है और यही प्रेम प्रेमा-भक्ति में परिणत हो जाता है। इस स्थिति में भक्तों को ईश्वर का ज्ञान होता है और तब उनमें ईश्वर के प्रति आसक्ति का उदय होता है। तत्पश्चात् वे ईश्वर-प्राप्ति के लिए स्वयं में एक प्रबल संवेग विकसित कर लेते हैं। यह प्रेम तथा आसक्ति की परिपक्वावस्था है जिसे व्यसन कहा जाता है। यह व्यसन भक्तों को सर्वोच्च आनन्द की सम्प्राप्ति की दिशा में उन्मुख करता है।
जब श्रीकृष्ण के प्रति भक्त का प्रेम गहनतम हो जाता है, तब वह सर्वत्र उनका दर्शन करने लगता है। अतः प्रत्येक वस्तु उसके प्रेम का पात्र हो जाती है और प्रत्येक वस्तु के साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। गोपियों को यह भाव प्राप्त था। वे सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करती थीं, यहाँ तक कि वे स्वयं को ही कृष्ण समझती थीं। यह सर्वोच्च अथवा परा-भक्ति है जो वेदान्तियों अर्थात् ज्ञानियों के ज्ञान के समकक्ष है। इस प्रकार के भक्तों के लिए समस्त आन्तरिक तथा बाह्य जगत् कृष्णमय अथवा पुरुषोत्तममय हो जाता है। इस भक्ति के फलस्वरूप भक्त श्रीकृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाता है।
मुक्ति सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। भगवान् कृष्ण की नित्य सेवा एवं दिव्य वृन्दावन में उनकी लीला में सम्मिलित होना ही चरम लक्ष्य है। जिनमें व्यसन अर्थात् ईश्वर के प्रति तीव्रतम अनुराग है, वे चतुर्विध मुक्ति को हेय समझ कर उनका परित्याग कर देते हैं। मर्यादा-भक्ति-मार्गियों को सायुज्य-मुक्ति प्राप्त होती है अर्थात् वे श्रीकृष्ण के साथ एकाकार हो जाते हैं। पुष्टि-भक्ति-मार्गी भक्त मुक्ति को अस्वीकार कर श्रीकृष्ण की लीला में सहभागी बनते हैं। उनके लिए श्रीकृष्ण की नित्य सेवा ही अभीष्ट होती है जिसमें उन्हें आत्यन्तिक आनन्द की प्राप्ति होती है। भक्त गौ, पक्षी, वृक्ष तथा नदियों का रूप ग्रहण कर श्रीकृष्ण के साहचर्य-जनित असीम आनन्द में मग्न रहते हैं। श्रीकृष्ण ने जो लीलाएँ व्रज तथा वृन्दावन में की थीं वैसी ही लीलाएँ ये भी हैं। कुछ भक्त दिव्य वृन्दावन-धाम में गोप तथा गोपियों के रूप में इन लीलाओं में सम्मिलित होते हैं।
विभिन्न प्रकार के मुक्त जीव
मुक्त जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ सनक की भाँति मुक्त हैं, कुछ ईश्वर के नगर में रहते हुए भगवत्कृपा से मुक्ति प्राप्त करते हैं और कुछ स्वयं में पूर्ण प्रेम विकसित कर ईश्वर का साहचर्य-लाभ करते हैं।
श्री चैतन्य का अचिन्त्य-भेदाभेद-दर्शन
प्रस्तावना
श्री चैतन्य अर्थात् गौरांगदेव को निस्सन्देह उत्तर भारत का महानतम वैष्णव आचार्य कहा जा सकता है। उन्होंने वैष्णव-धर्म को एक नया रूप प्रदान किया। उनका जन्म बंगाल में सन् १४८६ में हुआ था।
चैतन्य विशाल-हृदय थे। उन्होंने इसलाममतावलम्बियों को भी उदारतापूर्वक अपनाया। उनके शिष्य हरिदास एक मुसलमान फकीर थे। नित्यानन्द ने चैतन्य-मत का प्रचार-प्रसार सुदूर भूखण्डों तक किया। कर्नाटक में महाराजा के वंशधर रूप, सनातन तथा उनके भ्रातृज जीव गोस्वामी, जो वहाँ से आ कर बंगाल में बस गये थे, संस्कृत के उद्भट विद्वान् थे। वस्तुतः यही तीन व्यक्ति चैतन्य-मत के आन्दोलन के जन्मदाता थे। जीव गोस्वामी और बलदेव ने इस मत को दार्शनिक आधार प्रदान किया। जीव गोस्वामीकृत 'सत्सन्दर्भ' और इस पर स्वयं-रचित उनका भाष्य 'सर्वसंवादिनी' तथा ब्रह्मसूत्र पर बलदेवकृत 'गोविन्दभाष्य' इस मत के दार्शनिक शास्त्रीय ग्रन्थ हैं। बलदेव का 'प्रमेय-रत्नावली' भी एक लोकप्रिय ग्रन्थ है। जीव गोस्वामी और बलदेव रामानुज तथा मध्व के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्हें ईश्वर, आत्मा, माया अर्थात् प्रकृति, शुद्ध सत्त्व तथा काल की सत्ता मान्य है।
जीव तथा जगत् ईश्वर से पृथक् होते हुए भी उस पर आश्रित हैं। वे न तो उससे अभिन्न हैं, न भिन्न। इनके पारस्परिक सम्बन्ध को अचिन्त्य-भेदाभेद कहा जाता है।
चैतन्य ईश्वरत्व के एकत्व पर बल देते हैं जो लोक-प्रचलित उपासना के लिए प्रयुक्त अनेक विग्रहों में सन्निहित है।
परम सत्ता
विष्णु परम तत्त्व है। वह प्रेम तथा अनुग्रह का ईश्वर है। वह अद्वितीय और सत्-चित्-आनन्द है। माया के गुणों से रहित होने के कारण वह निर्गुण तथा सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होने के कारण सगुण है। वह जगत् का उपादान तथा निमित्त कारण है। वह जगत् का सृष्टा, धारक तथा संहारक है। अपनी पराशक्ति के कारण वह जगत् का निमित्त कारण तथा अपरा एवं आद्य शक्ति के कारण उपादान कारण है।
ईश्वर की रहस्यमयी तथा अचिन्त्य शक्तियाँ
जिस प्रकार सूर्य में प्रकाश तथा अग्नि में ताप निहित है, उसी प्रकार भगवान् कृष्ण में रहस्यमयी तथा अचिन्त्य शक्तियाँ निहित हैं। इन शक्तियों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। ये ईश्वराश्रित हैं। ईश्वर तथा उसकी शक्तियों में भेदाभेद-सम्बन्ध है। चित्-शक्ति, जीव-शक्ति तथा माया-शक्ति-ईश्वर की ये तीन शक्तियाँ हैं। इन्हें क्रमशः अन्तरंग, तटस्थ तथा बहिरंग भी कहा जाता है। चित्-शक्ति तथा माया-शक्ति की मध्यवर्तिनी होने के कारण जीव-शक्ति को तटस्थ-शक्ति भी कहा जाता है।
सृष्टि-प्रक्रिया
वैकुण्ठ का उद्भव चित्-शक्ति से हुआ है। वैकुण्ठ में केवल शुद्ध सत्त्व है। यहाँ माया का प्रवेश असम्भव है और काल यहाँ अपनी संहारक शक्ति के प्रयोग में सर्वथा अक्षम है।
जीवों की सृष्टि ईश्वर की तटस्थ-शक्ति अर्थात् जीव-शक्ति से होती है। उसकी जीव-शक्ति उसकी स्वरूप-शक्ति पर अवलम्बित है।
ईश्वर महत् तत्त्व से जगत् की संरचना करता है। अप्रकट वेदों को प्रकट कर वह ब्रह्मा में इनके ज्ञान को संक्रमित कर देता है और सृष्टि के अन्य चरणों का भार उसको सौंप देता है। जीव गोस्वामी तथा बलदेव के मतानुसार जीव तथा प्रकृति ईश्वर की ही शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। ईश्वर के दृष्टिपात मात्र से माया स्पन्दित हो उठती है।
विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त प्रभु
परब्रह्म भगवान् कृष्ण स्वयं को ज्ञानियों के समक्ष ब्रह्म, योगियों के समक्ष परमात्मा तथा भक्तों के समक्ष अपनी समस्त विभूतियों, सौन्दर्य, माधुर्य एवं समस्त विशिष्टाताओं से युक्त भगवान् के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान् कृष्ण आत्माओं की आत्मा तथा जो कुछ भी यहाँ अस्तित्ववान् है, उसके स्वामी हैं। केवल किसी भक्त के लिए ही समस्त दैवी गुणों से युक्त सर्वोपरि सगुण परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान सम्भव है। भगवान् कृष्ण का रूप अद्वितीय है। वे अनन्त रूप धारण करते हैं।
मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, गय तथा कृष्ण लीलावतार है। इनके अतिरिक्त गुणावतार तथा मन्वन्तरावतार भी हैं। सनकादि चार कुमार, नारद, पृथु परशुराम, ब्रह्मा और बैकुण्ठ में शेष तथा अनन्त जो पृथ्वी को धारण करते हैं प्रमुख आवेशावतार हैं। वे ईश्वर की प्रत्यक्ष शक्ति से सम्पत्र हैं। सनक में ज्ञान-शक्ति, नारद में भक्ति-शक्ति, ब्रह्मा में सृजन-शक्ति, अनन्त में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति शेष में भगवत्सेवा की शक्ति, पृथु में संसार की पोषण-शक्ति तथा परशुराम में दुष्टों के संहार की शक्ति निहित है।
राधा-कृष्ण
परम तत्त्व तथा अवतार अभिन्न हैं। वैयक्तिक आत्मा की भाँति वे अंश नहीं है। परमात्मा असंख्य रूप धारण करता है जिसमें कृष्ण सर्वप्रमुख हैं। राधा कृष्ण की अह्लादिनी-शक्ति हैं। परमात्मा समस्त आत्माओं का नियन्ता तथा सर्वव्यापी है।
जीव
जीव अणु आकार का है। वह ईश्वर का नित्य सेवक है। ईश्वर से उसका वही सम्बन्ध है जो रश्मियों का सूर्य से और स्फुलिंग का अपने स्रोत अग्नि-पुंज से है किन्तु सूर्य से विकीर्ण एवं उसका एक अंश होने पर भी रश्मि सूर्य नहीं होती। इसी प्रकार जीव जो अपने चेतन स्वरूप के कारण अंशतः ईश्वर-सदृश तथा अपनी जैविक प्रकृति तथा माया के प्रभाव के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण उससे भित्र है. ईश्वर नहीं है।
जीव माया के शक्ति-पाश में आबद्ध है। माया के कारण उसे अपने मूलभूत तथा दिव्य स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। मायाग्रस्त जीव को स्वभावर भगवान् कृष्ण का ज्ञान नहीं हो पाता। अतः भगवान् कृष्ण ने अपनी अनन्त करणा के वशीभूत हो कर वेदों की सृष्टि की है। वह शास्त्रों, गुरु तथा अन्तर्ज्ञान के माध्यम से स्वयं को जीवों के समक्ष प्रकट करता है और तब जीव को विश्वास हो जाता है कि भगवान् कृष्ण उसके स्वामी तथा रक्षक हैं।
भगवान् कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम द्वारा जीव को ईश्वरानुभूति हो सकती है। भक्ति से कर्म-विपाक का क्षय हो जाता है। यह चरम मोक्ष का साधन है। जीव भक्ति पूर्ण ईश्वर के सदृश हो सकता है; किन्तु वह उसमें तिरोहित नहीं हो सकता। जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।
भक्ति की संस्कृति
चैतन्य के उपदेशानुसार उत्कट तथा आत्यन्तिक प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति सम्भव है। कर्म में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति की सम्भावना के सम्बन्ध में राजा के एक मन्त्री द्वारा लिखे गये एक पत्र के उत्तर में उन्होंने लिखा था- "जिस प्रकार एक भ्रष्ट नारी अपने घर में रहते हुए भी अपने जार के चिन्तन में निरन्तर लीन रहती है, उसी प्रकार आप भी अपने विहित कर्मों को करते हुए मौन-भाव से निरन्तर भगवान् का ध्यान किया करें।"
चैतन्य के मतानुसार भक्ति के संस्कार से तन्मयता का उदय होता है और तन्मयता की गहनता ही प्रेम है।
रुचि से आसक्ति और आसक्ति से कृष्ण के प्रति रति-भाव का बीजारोपण होता है और जब इस संवेग में तीव्रता आती है, तब यह प्रेम का रूप ग्रहण कर लेता है। कृष्ण-भक्ति का यह स्थायी स्वरूप है।
जिस प्रकार दही में चीनी, कालीमिर्च और कपूर मिला देने से अत्यन्त सुस्वादु रसाल तैयार हो जाता है, उसी प्रकार स्थायी-भाव में रस के मिश्रण से वह विभाव, अनुभाव, सात्त्विक-भाव तथा व्यभिचारी-भाव में परिणत हो जाता है। आलम्बन तथा उद्दीपन विभाव के ये दो प्रकार हैं। आलम्बन कृष्ण आदि से तथा उद्दीपन उनकी वंशी-ध्वनि आदि से उद्दीप्त होता है। मुस्कान, नृत्य तथा संगीत अनुभाव को उद्दीप्त करते हैं। मूर्च्छा एवं अन्य संवेदनाएँ सात्त्विक-भाव के अन्तर्गत आती हैं। हर्ष, उल्लास आदि व्यभिचारी-भाव तैंतीस प्रकार के होते हैं।
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य-ये रस के पाँच प्रकार हैं। शान्त तथा दास्य रस में रति क्रमशः प्रेम तथा राग के स्तर तक जा पहुँचती है और सख्य तथा वात्सल्य अनुराग की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं।
कृष्ण-प्रेम : सर्वोच्च उपलब्धि
जिस भक्त में प्रेम का विकास हो चुका होता है, वह कृष्ण के साथ संलाप की स्थिति में रहता है। सांसारिक दुःख या क्लेश उसे क्षुब्ध नहीं कर पाते। लौकिक विषयों के प्रति वह आसक्त नहीं होता। वह निर्भय, भौतिक सफलताओं के प्रति निर्लिप्त तथा भगवान् कृष्ण के सामीप्य-लाभ के लिए लालायित रहता है।
कृष्ण-प्रेम सर्वोच्च प्राप्तव्य और भक्ति इसकी प्राप्ति का मुख्य साधन है। वस्तुतः कृष्ण-प्रेम जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। इससे भक्त कृष्ण की निष्काम सेवा में संलग्न होते और उसके रस के आनन्द का उपभोग करते हैं। भक्ति कृष्ण-प्राप्ति का एकमात्र साधन है; इसीलिए इसे अभिधेय या साधन कहा जाता है। जिस प्रकार धन से सुख की प्राप्ति होती है और सुखोपभोग से सांसारिक दैन्य स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति से कृष्ण-प्रेम का उद्भव होता है और इस प्रेमानुभूति से जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दुःख-निवृत्ति तथा पुनर्जन्म से मुक्ति प्रेम का परिणाम नहीं है। आत्यन्तिक रमणीयता अर्थात् मोक्ष प्रेम द्वारा ही सृजित है। अतः इस प्रेम को सर्वोच्च उपलब्धि की संज्ञा प्रदान की गयी है।
श्री चैतन्य के अन्य उपदेश
गुरु-भक्ति श्री चैतन्य के उपदेशों की मूलभूत विशिष्टता है। वेदों तथा भागवतपुराण आदि ग्रन्थों का स्वाध्याय तथा उनकी शिक्षाओं को हृदयंगम करना चाहिए। नैतिकता का अभ्यास तथा जीवों के प्रति दया, विनम्रता, चित्त-शुद्धि, ऐहिक इच्छाओं से मुक्ति, शान्ति तथा सत्य जैसे गुणों का विकास अनिवार्य है। जाति-भेद की भावना उपेक्षणीय है। कोई भी व्यक्ति भगवत्कृपा का अधिकारी हो सकता है।
करुणा, सत्य, साधुता, सरलता, दान, सज्जनता, शुद्धता, निर्वैर, विनम्रता, शान्ति, कोमलता, मैत्री तथा मौन जैसे गुणों से अलंकृत व्यक्ति वैष्णव होता है। वह सर्व-जन-हितैषी तथा भगवान् कृष्ण के ऊपर आश्रित होता है। वह निष्काम, मिताहारी तथा आत्मनिग्रही होता है। वह षड्रिपुओं को विजित कर चुका होता है। वह दूसरों का सम्मान करता है; किन्तु उसे दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं होती।
संकीर्तन : रामबाण औषधि
इस कलियुग में नाम-संकीर्तन रामबाण औषधि है। यह वैदिक यज्ञ के समकक्ष है। निष्ठावान् यजमान कृष्ण के चरणों के दर्शन से पुरस्कृत होता है। संकीर्तन पाप-नाश तथा विश्व-विजय की शक्ति प्रदान करता है। इससे आत्मा की परिशुद्धि और भक्ति की समस्त विधाओं का उद्भव होता है। देश तथा काल इसे प्रतिबन्धित नहीं कर पाते। इसका सुफल सर्वत्र प्राप्त होता है। यह सर्वशक्ति का पर्याय है।
हरि-नाम-कीर्तन उस व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जो निश्चित रूप से पद-मर्दित दूर्वा-पत्र से भी अधिक विनम्र हो और उस वृक्ष की भाँति धैर्यवान्, सहिष्णु तथा उदार हो जो अपने उच्छेद के समय भी क्रन्दन नहीं करता और तृषित होने पर भी जल की याचना नहीं करता; अपितु इसके विपरीत जो याचक के समक्ष अपने कोष को अनावृत कर देता है और जो ग्रीष्म तथा वर्षा को सहन करते हुए भी शरणागतों को ग्रीष्म तथा वर्षा से सुरक्षा प्रदान करता है। वस्तुतः हरि-नाम-संकीर्तन का वही अधिकारी है जो सम्मान का अधिकारी होते हुए भी समस्त प्राणियों में भगवान् को व्याप्त जान कर सबको सम्मानित करता है। इस प्रकार जो कृष्ण का नाम जप करता है, उसे कृष्ण के दिव्य प्रेम की सम्प्राप्ति होती है।
त्रयोदश अध्याय
(शैव-सिद्धान्त तथा शाक्त-मत)
शैव-सिद्धान्त-दर्शन
प्रस्तावना
जिन ग्रन्थों में शैव-मत की विवेचना की गयी है, उनमें नकुलीश पाशुपत, शैव, प्रत्यभिज्ञा तथा रसेश्वर-इन चार सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है।
शैव-सिद्धान्त दाक्षिणात्य-शैव-मत का दर्शन है। इसके प्रणयन का श्रेय किसी एक प्रणेता को नहीं दिया जा सकता। यह सिद्धान्त शंकर के अद्वैत तथा रामानुज के विशिष्टाद्वैत का मध्यवर्ती सिद्धान्त है। अट्ठाइस शैवागम, 'तिरुमूरै' नामक शैव-स्तोत्रों का संकलन, शैव-सन्तों के जीवन-चरित्र का 'पेरियपुराणम्' नामक संकलन, मेकण्डर का 'शिव-ज्ञान-बोधम्', अरुलनन्दीकृत 'शिव-ज्ञान-सिद्धियार' तथा उमापति की कृतियाँ इस साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ हैं। तिरुमूलर के ग्रन्थ 'तिरुमन्तिरम्' की नींव पर ही शैव-सिद्धान्त-दर्शन का परवर्ती प्रासाद निर्मित हुआ।
शैव-दर्शन के केन्द्रीय सिद्धान्त के अनुसार शिव यथार्थ सत्ता है तथा शिव और जीव में तत्त्वगत समानता होते हुए भी इनमें एकरूपता नहीं है। पति, पशु, पाश तथा छत्तीस तत्त्व विश्व के संघटक तत्त्व हैं जो यथार्थ हैं।
शैव-सिद्धान्त वेदान्त का विशुद्ध या परिमार्जित तत्त्व है। दक्षिण में इसका प्रचार-प्रसार ईसा पूर्व भी था। तिरुनेल्वेली और मदुरै शैव-मत के केन्द्र हैं। दक्षिण में शैव-मत आज भी अत्यन्त लोकप्रिय है। यह वैष्णव-मत का विरोधी है।
सर्वोच्च सत्ता के लक्षण
शिव को यथार्थ सत्ता कहा जाता है। वह असीम चेतना है। वह नित्य, निरंजन, निराकार, स्वतन्त्र, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, अद्वय, अनादि, अकारण, अनवद्य, स्वयंस्थित, चिरस्वतन्त्र, नित्य शुद्ध तथा पूर्ण है। वह कालातीत है। वह भूमा तथा अपरिमित प्रज्ञा है। वह सर्वदोषशून्य, सर्वकर्ता और सर्वज्ञाता है।
भगवान् शिव प्रेम के ईश्वर हैं। उनकी कृपा अपरिमेय एवं उनका प्रेम असीम है। वे रक्षक तथा गुरु हैं। वे जीवात्माओं को भौतिकता की दासता से मुक्त करने में सतत संलग्न रहते हैं। मनुष्य जाति के प्रति अपने उत्कट प्रेम के कारण वे गुरु का रूप धारण करते हैं। उनकी इच्छा है कि सभी लोग उनका ज्ञान प्राप्त कर आनन्दप्रद शिव-पद प्राप्त करें। वे जीवात्माओं की गतिविधि का पर्यवेक्षण करते हुए उनकी प्रगति में सहायक होते हैं। वे उन्हें पाश-मुक्त करते हैं।
भगवान् के पंच-कृत्य
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव एवं अनुग्रह-भगवान् की पंच-क्रियाएँ हैं जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर तथा सदाशिव द्वारा सम्पन्न की जाती हैं।
शिव, शक्ति और माया
भगवान् शिव अपनी शक्ति के माध्यम से समस्त जगत् में परिव्याप्त हैं। अपनी शक्ति से वे अपने व्यापार का सम्पादन करते हैं। शक्ति भगवान् शिव की चेतन शक्ति तथा उनकी देह है। कुम्भकार कुम्भ का प्रथम कारण, दण्ड तथा चक्र इसके उपकरण तथा मृत्तिका इसका उपादान कारण है। इसी प्रकार भगवान् शिव जगत् के आदि कारण, शक्ति इसका उपकरण तथा माया उपादान कारण है।
चैतन्य-स्वरूप होने के कारण शक्ति जगत् का उपादान कारण नहीं है। शिव विशुद्ध चेतना है; किन्तु प्रकृति सर्वथा अचेतन है। शक्ति इनके मध्य का संयोजन-सूत्र है।
शक्ति शिव का प्रतिबिम्ब है। इसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। मनुष्य-जाति के प्रति अपने प्रेम की अतिशयता के कारण शिव यह स्वरूप धारण करते हैं। वे सर्व-जन-ज्ञेय हों, यह उनकी अभीप्सा है।
शुद्ध माया से तत्त्वों का विकास
जागतिक विकास के मूल में जीवात्माओं का कल्याण निहित है। उनकी मुक्ति ही सृष्टि की प्रत्येक प्रक्रिया का उद्देश्य है। जगत् यथार्थ एवं नित्य है। जड़ जगत् तथा आत्माएँ भगवान् शिव की देह के संघटक तत्त्व हैं।
शैव-सिद्धान्त सांख्य के पचीस तत्त्वों के विपरीत विश्व का विश्लेषण छत्तीस तत्त्वों में करता है। इन छत्तीस तत्त्वों का प्रादुर्भाव माया से होता है जो जगत् का उपादान कारण है। शुद्ध माया अपनी आद्यावस्था में माया है। इससे पाँच शुद्ध तत्वों-शिव-तत्व, शक्ति-तत्व,शिवसदाशिव तत्वों और तत्व तथा शुद विद्या-तत्त्व का प्रादुर्भाव होता है। शिव इन पाँच तत्त्वों द्वारा अपने व्यापार में प्रवृत होते हैं।
माया का विकास सर्वप्रथम सूक्ष्म तत्त्वों में और तत्पश्चात् स्थूल तत्त्वों में होता है। शिव-तत्त्व समग्र चेतना तथा क्रिया का अधिष्ठान है। यह निष्कल है। अपनी शक्ति के क्रियाशील होने पर शिव भोक्ता हो जाते हैं और तब उन्हें सदाशिव और सदाख्य के नाम से अभिहित किया जाता है, जो वस्तुतः शिव से भिन्न नहीं है। शुद्धाविद्या ज्ञान का हेतु है।
आत्मा को आबद्ध करने वाले पाश आणव, कर्म तथा माया
आत्माएँ (पशु) भगवान् शिव (पति) की भाँति स्वभावतः असीम, सर्वव्यापी, नित्य तथा सर्वज्ञ हैं; किन्तु वे अपने को सान्त, सीमित, अल्पज्ञ एवं नश्वर समझाती हैं। ऐसा उनके पाश, जिन्हें आणव, कर्म तथा माया कहते हैं, के कारण होता है। इन्हें मल-त्रय कहते हैं। आणव वह कषाय है जो सर्वव्यापी जीव को स्वयं को अणु समझाने के लिए विवश करता है। इससे परिच्छिन्नता की भ्रान्त धारणा का प्रादुर्भाव होता है। दूसरा मल या पाश कर्म है। आत्मा अपनी सीमाओं के कारण एक विशेष रूप में सक्रिय हो कर शुभ तथा अशुभ कर्मों का सम्पादन करती है। कर्म के कारण आत्मा का देह से संयोग होता है। संसार में अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। कर्म-फल-भोग तथा ज्ञान की सम्प्राप्ति के लिए संसार तथा शरीर का अस्तित्व आवश्यक है। तृतीय मल अथवा पाश माया है जो इन उपकरणों की आपूर्ति करती है। माया जगत् का उपादान कारण है। इससे अनुभव तथा सीमित ज्ञान की प्राप्ति होती है।
आत्मा को दीर्घ अनुभव से यह ज्ञान होता है कि संसार दुःखमय तथा नश्वर है और उसे शिवत्व या शिव के साथ एकरूपता के माध्यम से ही शाश्वत आनन्द तथा अमरत्व की उपलब्धि हो सकती है। तब उसमें वैराग्य तथा नित्यानित्य-विवेक का विकास होता है।
जीवों के तीन क्रम
शैव-सिद्धान्त के प्रवर्तकों ने जीवों तथा पशुओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। इनको विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा सकल कहते हैं। विज्ञानाकल जीवों में केवल आणव मल रहता है। ये माया तथा कर्म की मलिनता से मुक्त हो चुके होते हैं।
प्रलयाकल जीव प्रलय के समय केवल माया से मुक्त रहते हैं और सकल जीवों में आणव, कर्म तथा माया-ये तीनों मल विद्यमान रहते हैं। मल-त्रय से केवल जीव प्रभावित होते हैं। शिव इनके प्रभाव से सर्वथा
असम्पृक्त रहते हैं। जो इन मलों से मुक्त हैं, उन्हें शिवत्व तथा शिव की सादृश्यता की सम्प्राप्ति होती है और उन्हें सिद्ध अथवा पूर्णत्व-प्राप्त जीव कहा जाता है।
शिवत्व अर्थात् ईश्वर-साक्षात्कार का मार्ग
यदि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्वपापमूलामाया, पुनर्जन्म के कारण-भूत कर्म तथा जीव की परिच्छिन्नता की भ्रान्तिजन्य अवधारणा का प्रहाण एक अनिवार्य आवश्यकता है।
कठोर तप, समुचित अनुशासन तथा गुरु कृपा से पाश-त्रय का प्रहाण सम्भव है; किन्तु इसके लिए सर्वाधिक अपेक्षित है शिव का अनुग्रह। चर्या, क्रिया तथा योग (यम-नियमादि) अनुशासन के संघटक तत्त्व हैं। जब साधक चर्या, क्रिया तथा योग का निष्ठापूर्वक अभ्यास करता है, तब उसे शिव-कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान् शिव तब उसे उद्बुद्ध करते तथा उसके समक्ष स्वयं को अनावृत करते हुए उसे ज्योतिर्मय कर देते हैं। इसके फल-स्वरूप आत्मा को शिव के साथ तद्रूपता अर्थात् शिवत्व का पूर्ण बोध हो जाता है।
अनुशासन तथा अनुग्रह की परिणति ज्ञान में होती है। ज्ञान मुक्ति अथवा दिव्य सौन्दर्य की प्राप्ति का सर्वोच्च साधन है। कर्म तथा अन्य मार्ग इसके सहायक तथा पूरक मात्र हैं।
शिवत्व की सम्प्राप्ति का अर्थ जीव का शिव में आत्यन्तिक तिरोभाव नहीं है। मुक्त आत्मा अपने पृथक् व्यक्तित्व से वंचित नहीं होता। वह भगवान् में अन्तर्भूत आत्मा के रूप में सतत विद्यमान रहता है। भेद के साथ-साथ तात्त्विक एकत्व की महासम्बोधि ही शिवत्व है। आत्मा को शिव का स्वरूप तो प्राप्त हो जाता है; किन्तु वह स्वयं शिव नहीं हो पाता।
शक्ति-योग-दर्शन
प्रस्तावना
शक्ति-योग-दर्शन में शिव सर्वव्यापी, निर्वैयक्तिक तथा निष्क्रिय हैं। वे शुद्ध चैतन्य हैं। शक्ति गत्यात्मिका है। शिव तथा शक्ति प्रकाश तथा विमर्श की भाँति परस्पर संयुक्त हैं। शक्ति अथवा विमर्श विशुद्ध चैतन्य में अन्तर्भूत शक्ति है। विमर्श से भेदमूलक संसार की उत्पत्ति होती है। शिव चित् तथा शक्ति चिद्रूपिणी है। ब्रम्हा, बिष्णु तथा शिव शक्ति के आदेशानुसार अपने-अपने कार्य क्रमशः सृष्टि, स्थिति तथा संहार में प्रवृत्त होते हैं। शक्ति इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया से सम्पत्र है। शिव तथा शकि एक है। शक्ति-तत्त्वं तथा शिव-तत्त्व अविभाज्य हैं। शिव तथा शक्ति में नित्य सम्बन्ध है।
शिव-तत्त्व तथा शक्ति-तत्त्व
परम शिव का सृजनात्मक पक्ष शिव-तत्त्व है। शक्ति-तत्त्व शिव का संकल्प है। वह समस्त जगत् का बीज तथा गर्भाशय है।
शिव के दो पक्ष हैं। प्रथम पक्ष में वह सर्वोच्च तथा अपरिवर्तनीय सच्चिदानन्द है। वह परा संवित् है। निष्कल शिव निर्गुण शिव है। वह सृजनात्मक शक्ति से सम्बद्ध नहीं है। अपने द्वितीय पक्ष में वह जगत् के रूप में परिणत हो जाता है। इस परिवर्तन का कारण शिव-तत्त्व है। शक्ति-तत्त्व ब्रह्म का प्रथम गत्यात्मक स्वरूप है। शिव-तत्व तथा शक्ति-तत्त्व परस्पर अविभाज्य हैं।
शक्ति : माया की नियामिका
माया अथवा प्रकृति शक्ति के गर्भ में स्थित है। माया जगत् का गर्भाशय है। प्रलय-काल में माया प्रच्छन्न रूप में विद्यमान रहती है; किन्तु सृजन में वह गत्यात्मक हो जाती है। शक्ति से निर्देशित माया अनेक भौतिक तत्त्वों तथा चेतन प्राणियों के भौतिक अवयवों के रूप में प्रादुर्भूत होती है।
शाक्त-दर्शन में छत्तीस तत्त्वों का उल्लेख है।
शक्ति : सर्वव्यापी ब्रह्म का सक्रिय स्वरूप
शक्ति सर्वान्तर्यामी ईश्वर का क्रियात्मक स्वरूप है। शिव या ब्रह्म अपरिवर्तनीय चेतना है। शक्ति उसका परिवर्तनशील पक्ष है जो मन तथा पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त होता है। वह इस पक्ष की मूर्त रूप तथा जागतिक प्रपंच की संचालिका है। ईश्वरीय लीला उसी के संचालन में सम्पन्न होती है। वह जगत् की धारिका है। यह संसार उसी सर्वोच्च शक्ति पर आश्रित है। वह ब्रह्माण्ड की जननी है। वह जगन्माता, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, चण्डी, चामुण्डी, त्रिपुरसुन्दरी और राजराजेश्वरी है। उसे ललिता, कुण्डलिनी और पार्वती भी कहते हैं, जिस प्रकार अधि तथा उसकी दाहिका-शक्ति में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर तथा उसकी शक्ति में भी कोई भेद नहीं है।
देवी भगवान् शिव की शक्ति है। वह जड़-शक्ति तथा चित्-शक्ति है। प्रकृति जड़-शक्ति और शुद्ध माया चित्-शक्ति है। नाद, बिन्दु तथा अन्य तत्त्व शक्ति के विभिन्न पक्षों के नाम हैं। शक्ति की प्रकृति, माया, महामाया तथा श्रीविद्या है। शक्ति स्वयं ही ब्रह्म है। वह स्वयं को शिव के समक्ष दश महाविद्याओं-काली, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, मातंगी, षोडशी, धूमावती, त्रिपुरसुन्दरी, तारा और भैरवी - के रूप में अभिव्यक्त करती है।
शक्ति चिरूपिणी है। वह विशुद्ध तथा आनन्दमयी चेतना है। वह प्रकृति की जननी है। वह जगज्जननी, सृष्टि की उद्भाविका, महिषासुरमर्दिनी, भ्रान्ति-नाशिनी, अविद्या-नाशिनी तथा दारिद्र्य-नाशिनी है।
जगत् शक्ति की अभिव्यक्ति है। असंख्य ब्रह्माण्ड दिव्य माता की मात्र चरण-धूलि हैं। उसकी महिमा अपार, उसकी दिव्य दीप्ति अवर्णनीय तथा उसकी महानता अपरिमेय है। वह अपने निष्ठावान् भक्तों पर कृपा-वृष्टि करती है। वह वैयक्तिक आत्मा को एक चक्र से दूसरे चक्र तथा एक भूमिका से दूसरी भूमिका की ओर उन्मुख कर उसे सहस्रार में भगवान् शिव के सायुज्य से कृतार्थ करती है।
दिव्य माता की अभिव्यक्तियाँ
सर्वोच्च अधिपति स्वयं को शिव के रूप में तथा अपनी शक्ति को अपनी पार्श्ववर्तिनी दुर्गा या काली के रूप में प्रकट करता है। जिस प्रकार पति-पत्नी परिवार के कुशल-क्षेम के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उसी प्रकार भगवान् शिव तथा शक्ति जगत् के परिरक्षण में संलग्न रहते हैं।
दिव्य माता सर्वत्र त्रिगुणमयी हैं। वे तीन गुणों-सत्त्व, रजस् और तमस् से सम्पन्न हैं। वे स्वयं को इच्छा-शक्ति, क्रिया-शक्ति तथा ज्ञान-शक्ति के रूप में अभिव्यक्त करती हैं। वे ब्रह्मा के संयोग से ब्रह्मा-शक्ति सरस्वती, विष्णु के संयोग से विष्णु-शक्ति लक्ष्मी तथा शिव के संयोग से शिव-शक्ति गौरी हैं। अतः उन्हें त्रिपुरसुन्दरी कहा जाता है।
राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री-प्रकृति अथवा देवी के ये पाँच आद्य रूप हैं। दुर्गा ने विष्णु के माध्यम से मधु और कैटभ का, महालक्ष्मी के रूप में महिषासुर का और सरस्वती के रूप में शुम्भ तथा निशुम्भ का उनके सहकर्मियों धूमलोचन, चण्ड, मुण्ड तथा रक्तबीज सहित संहार किया।
दिव्य माता का धाम
श्रीनगर दिव्य माता त्रिपुरसुन्दरी का धाम है। मणिद्वीप नामक यह भव्य धाम पचीस परकोटों से परिवृत है जो पचीस तत्त्वों के प्रतीक हैं। दीप्तिमान् चिन्तामणि राजभवन मध्य में स्थित है। दिव्य माता उस अद्भुत दिव्य भवन में श्रीचक्र-स्थित बिन्दु-पीठ में विराजमान् हैं। उनके लिए एक ऐसा ही धाम जीव के शरीर में भी हैं।
देह शक्ति है। देह की आवश्यकताएँ शक्ति की आवश्यकताएँ हैं। जीव के सुख-भोग को शक्ति स्वयं उसी के माध्यम से भोगती है। यह उसके नेत्रों से देखती, उसके हाथों से कार्य करती तथा उसकी कर्णेन्द्रियों से श्रवण करती है। शरीर, मन, प्राण, अहं, बुद्धि, अंग तथा सारे व्यापार उसी की अभिव्यक्तियाँ हैं।
अखिल ब्रह्माण्ड उसका शरीर है। पर्वत उसकी अस्थियाँ, नदियाँ उसकी शिराएँ, समुद्र उसका मूत्राशय, सूर्य-चन्द्र उसके नेत्र, वायु उसकी साँस तथा अग्नि उसका मुख है।
देवी की अवर्णनीय महिमा यक्ष की कथा
केनोपनिषद् में कहा गया है कि देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर अहंकार-ग्रस्त हो गये। उन्होंने भ्रान्तिवश इस सफलता को अपने ही शौर्य तथा शक्ति या परिणाम मान लिया। भगवान् ने उनके भ्रम-निवारण के लिए उन्हें एक सीख देने का निश्चय किया। वे उनके समक्ष एक महाकाय यक्ष, जिसका आदि-अन्त अद्रष्टव्य था, के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने उस यक्ष का परिचय प्राप्त करने के लिए उसके पास अग्नि को भेजा। यक्ष ने अग्नि से पूछा- "तुम्हारा नाम और तुम्हारी शक्ति क्या है?" अग्नि ने उत्तर दिया- "मैं जातवेदा अग्नि हूँ और अखिल ब्रह्माण्ड को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ।" यक्ष ने उसके समक्ष एक शुष्क तृण रख कर उसे जलाने को कहा; किन्तु अग्नि उसे जला नहीं सका और लज्जित हो कर वहाँ से चला गया। इसके पश्चात् देवताओं ने उसके पास वायु को भेजा। यक्ष ने उससे पूछा- "तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति क्या है?" वायु ने कहा- "मैं वायु देव हूँ और इस ब्रह्माण्ड को एक क्षण में उड़ा सकता हूँ।" तब यक्ष ने उसके सम्मुख एक शुष्क तृण रखते हुए उसे उड़ाने की चुनौती दी। किन्तु, वायु उसे एक इंच भी नहीं हिला सका और वह भी लज्जित हो कर वहाँ से चला गया। अन्त में स्वयं इन्द्र आये जिन्हें देखते ही यक्ष अन्तर्धान हो गया।
तत्पश्चात् इन्द्र के सम्मुख उमा प्रकट हुई और उन्हें यक्ष का यथार्थ परिचय देते हुए कहा - "देवताओं को विजय-श्री अपनी शक्ति से नहीं, दिव्य माता की शक्ति से प्राप्त हुई है। देवताओं की शक्ति का स्रोत उमा अथवा कृष्ण की सहोदरा हैमवती है।" शक्ति ज्ञान का महान् गुरु है। वह अपने भक्तों को ज्ञान से समृद्ध करती है।
देवताओं की पृष्ठभूमि में देवी
विष्णु तथा महादेव द्वारा अनेक असुरों के संहार के मूल में देवी की ही शक्ति निहित थी। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र को अपने-अपने व्यापार क्रमशः सृष्टि, पोषण तथा संहार में प्रवृत्त होने के लिए देवी ने ही शक्ति प्रदान की थी। वह ब्रह्माण्डीय जीवन के केन्द्र में स्थित है। उसकी अवस्थिति हमारे शरीरस्थ मूलाधार चक्र में है। वह सुषुम्ना के माध्यम से शरीर को सम्पुष्टि प्रदान करती है। मेरु पर्वत के शिखर पर विराजमान दिव्य माता से अखिल विश्व को संजीवनी शक्ति की सम्प्राप्ति होती है।
माता का संरक्षक रूप
शक्ति उस तत्त्व का पर्याय है जो विश्व में हमारे अस्तित्व का कारण है। इस संसार में बालक की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति माता ही करती है। बालक की संवृद्धि, उसके विकास तथा उसके पोषण की व्यवस्था वही करती है। इसी प्रकार जीवन की समस्त आवश्यकताओं, इसके कार्यकलाप तथा इनके कार्यान्वयन की क्षमता के लिए हम जगज्जननी शक्ति माता पर ही निर्भर हैं।
सद्योजात शिशु के मुख से प्रथम निःसृत शब्द प्रिय जननी का नाम, माँ ही होता है। क्या कोई ऐसा बालक हो सकता है जो अपनी माता द्वारा प्राप्त स्नेह के लिए उसका ऋणी न हो? आपको माता से ही सुरक्षा, सान्त्वना, हर्ष तथा परिचर्या की सम्प्राप्ति होती है। जीवन-पर्यन्त वही आपकी मित्र, शुभ-चिन्तक, गुरु तथा पथ-प्रदर्शिका है। समस्त स्त्रियाँ दिव्य माता का प्रकट स्वरूप हैं।
शाक्त-मत के ग्रन्थ
ऋग्वेद का देवीसूक्त, श्रीसूक्त, दुर्गासूक्त, भूसूक्त, नीलासूक्त तथा शाक्त-मत का अनुमोदन करने वाले त्रिपुरसुन्दरी उपनिषद्, सीतोपनिषद्, देवी उपनिषद्, सौभाग्योपनिषद्, सरस्वती उपनिषद् परमेश्वर के मातृस्वरूप की दृढ़तापूर्वक उद्घोषणा करते हैं।
शाक्त-मत : एक सार्वजनीन मत
ईश्वर को मातृ-रूप मान कर जो सृष्टिकत्री, पालनकर्त्री तथा संहारकत्री महाशक्ति की उपासना करता है, वह शाक्त है।
शक्ति की उपासना अथवा शाक्त-मत संसार के प्राचीनतम तथा सर्वाधिक व्यापक धर्मों में है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति में प्रभुता अथवा शक्ति की अभीप्सा है। शक्ति-प्राप्ति से वह उल्लसित हो उठता है। उसमें दूसरों को पराभूत करने की कामना जाग्रत हो जाती है। युद्ध प्रभुता की लोलुपता के परिणाम हैं। वैज्ञानिक शाक्त-मत के अनुयायी हैं। जो कोई भी इच्छा-शक्ति के विकास तथा आकर्षक व्यक्तित्व का आकांक्षी है, वह शाक्त-मत का अनुयायी है। वस्तुतः इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति शाक्तमतावलम्बी है।
आधुनिक वैज्ञानिकों के कथनानुसार प्रत्येक वस्तु मात्र ऊर्जा है जो पदार्थ के समस्त प्रारूपों का भौतिक सारतत्त्व है; किन्तु शाक्त-दर्शन के अनुयायियों ने ऐसा बहुत पहले ही कह दिया था। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा था कि ऊर्जा असीम तथा सर्वोच्च शक्ति अर्थात् महाशक्ति की सीमित अभिव्यक्ति है।
वेदान्त तथा शक्तिवाद
शाक्त-मत वेद पर आधारित है। शाक्त-मत के अनुसार ब्रह्म के अनुभवातील एवं अतीन्द्रिय स्वरूप जैसे विषयों का मूल स्रोत तथा प्रमाण वेद हैं। शक्तिवाद या शाक्त-दर्शन अद्वैतवाद का ही एक प्रारूप है। शाक्त-मत वेदान्त ही है। शाक्तों तथा वेदान्तियों की आध्यात्मिक अनुभूतियों में साम्य के दर्शन होते हैं।
शाक्तों की आस्था ब्रह्म के मूर्त एवं अमूर्त, दोनों रूपों के प्रति है। ब्रह्म निष्कल अर्थात् प्रकृति से असम्पृक्त है; किन्तु इसके साथ ही वह सकल अर्थात् प्रकृति से सम्पृक्त भी है। वेदान्ती भी निरुपाधिक अर्थात् माया-विरहित विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म के साथ-साथ सोपाधिक अर्थात् माया-विशिष्ट सगुण ब्रह्म के प्रति भी अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। बात एक ही है। भेद केवल नाम का है और यह नामान्तर शब्द-जाल मात्र है। लोग शब्दों के प्रश्न पर वाग्युद्ध करते, बाल की खाल निकालते एवं तर्क-वितर्क तथा बौद्धिक व्यायाम का प्रदर्शन करते हैं। यथार्थतः सारभूत तत्त्व एक ही है। मृत्तिका ही सत्य है। उससे निर्मित घटादि नाम-रूप मात्र हैं। निर्गुण ब्रह्म में शक्ति प्रच्छन्न और सगुण ब्रहा में गत्यात्मक है।
शक्तियोग-साधना
शाक्तवाद एक सिद्धान्त या दर्शन मात्र नहीं है। इसमें साधक की प्रकृति, क्षमता और उसके विकास के स्तर के अनुरूप नियमित अनुशासन तथा योग-साधना को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। शक्ति का उन्मेष साधना का प्राप्तव्य है। शाक्त-साधना कुण्डलिनी की जाग्रति एवं शक्ति के साथ शिव के सायुज्य तथा तज्जनित सर्वोच्च आनन्द अथवा निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति में साधक को योगदान देती है। यह शरीरस्थ शक्तियों को जाग्रत कर शिव-शक्ति-सायुज्य में सहायक सिद्ध होती है। जब साधक षड्चक्र-भेदन तथा कुण्डलिनी को जाग्रत करने में समर्थ होता है, तब उसे सिद्धि-प्राप्ति हो जाती है। साधन-विधि साधक की मनोवृत्तियों तथा क्षमता पर निर्भर है।
भाव अथवा प्रवृत्ति
साधक सोचता है कि विश्व तथा दिव्य माता में एकरूपता है। वह स्वयं को शक्ति-स्वरूप मान कर सर्वत्र एकरूपता का दर्शन करने लगता है। उसे दिव्य माँ अर्थात् शक्ति तथा ब्रह्म की एकात्मकता की अनुभूति होने लगती है।
उच्चस्तरीय साधक को अनुभव होता है कि वह देवी है और देवी उसमें है। वह किसी बाह्य विषय की उपासना के स्थान पर स्वयं को देवी मान कर अपनी ही उपासना करता है। वह कह उठता है-"सो ऽहम्" अर्थात् मैं ही वह (देवी) हूँ।
कुण्डलिनी की जागृति
शक्ति की जागृति के लिए ध्यान, भाव, जप तथा मन्त्र-शक्ति अनिवार्य है। पचास अक्षरों की मूर्त-स्वरूपा माता विभिन्न चक्रों में विभिन्न अक्षरों में विद्यमान है। वाद्ययन्त्रों को ताल-सुर की समस्वरता के साथ बजाने पर मधुर संगीत की सृष्टि होती है। इसी प्रकार अक्षरों के तारों पर क्रमिक आघात से षड्चक्रों में विद्यमान देवी, जो अक्षरों का सारतत्त्व है, जाग्रत हो जाती है। उसकी जागृति के फलस्वरूप साधक को सहज ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह कहना कठिन है कि वह कब, कैसे और किस साधक को दर्शन देती है।
जीव को कुण्डलिनी की सुप्तावस्था में संसार का आभास हुआ करता है। उसमें वस्तुगत चेतना विद्यमान रहती है; किन्तु कुण्डलिनी के जाग्रत होने पर जीव सुस्तवस्था को प्राप्त हो जाता है। उसकी जागतिक चेतना सह हो जाती है और वह सुपावर के साथ तादात्तय-सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। समाधिस्थ साधक के शरीर का परिरक्षण सहसार में शिव-शक्ति-सायुज्य से निःसृत अमृत से होता है।
पशु-भाव तथा दिव्य भाव
स्त्री के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थूल मैथुन है। इसका कारण पशु-भाव अर्थात् पाशविक प्रवृत्ति है। निर्विकल्प समाधि में माँ कुण्डलिनी शक्ति सहस्रार में शिव के साथ तद्रूप हो जाती है। यही यथार्थ मैथुन अर्थात् आनन्दमय सायुज्य है जो दिव्य भाव की परिणति है। सत्संग, गुरु-सेवा, त्याग, वैराग्य, विवेक, जप तथा ध्यान के माध्यम से पशु-भाव से दिव्य भाव की ओर आरोहण आपकी अनिवार्य आवश्यकता है।
गुरु के दिशा-निर्देश तथा दैवी कृपा की अपरिहार्यता
शक्ति-योग-साधना किसी सिद्ध गुरु के दिशा-निर्देशन में पूर्ण तथा तत्परता के साथ विधिपूर्वक करनी चाहिए। शक्ति-साधना के लिए गुरु आवश्यक है। वे साधक को दीक्षित कर उसमें दिव्य शक्ति का संचार करते हैं।
दैवी कृपा से वंचित किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक तथा जागतिक प्रपंच-पाश से मुक्त होना असम्भव है। माया के बन्धन को विच्छिन्न करना अत्यन्त दुष्कर है। यदि आप शक्ति की उपासना दिव्य माता के रूप में करते हैं, तो आप उसके अनुग्रह तथा आशिष से प्रकृति से अत्यन्त सरलतापूर्वक असम्पृक्त हो सकते हैं। वह आपके मार्ग के समस्त व्याघातों को विनष्ट कर आपको सुरक्षित रूप में अन्तहीन आनन्द के ज्योतिर्मय लोक में पहुँचा देगी, जिसके फल-स्वरूप आप पूर्णतः पाश-मुक्त हो जायेंगे। जब वह प्रसन्न हो कर आपको अपनी कृपा से कृतकृत्य करेगी, तभी आपको इस भयावह भव-बन्धन से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी।
शक्ति का ज्ञान मुक्ति की ओर उन्मुख करता है
शक्ति के ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। शिव देवी से कहते हैं: "शक्तिज्ञानं विना देवि निर्वाणं नैव जायते- हे देवी, शक्ति के ज्ञान के बिना मुक्ति की सम्प्राप्ति असम्भव है।" मायाग्रस्त जीव स्वयं को कर्ता तथा भोक्ता मान कर शरीर से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। शक्ति के अनुग्रह तथा साधना अर्थात् आत्म-संस्कृति के माध्यम से जीवात्मा स्वयं को सर्व-पाश-मुक्त कर आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि प्राप्त करता और अपने को सर्वोपरि सत्ता में विलीन कर देता है।
देवी की कृपा की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना, उत्कट आस्था, पूर्ण भक्ति तथा आत्म-समर्पण आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। उसकी कृपा से ही आपको उस शाश्वत सत्ता का ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
जगज्जननी त्रिपुरसुन्दरी की जय हो ! वही राजराजेश्वरी तथा ललितादेवी हैं। आप सबको उनका आशिष प्राप्त हो! आप सब शक्ति अर्थात् जगज्जननी का अनुग्रह प्राप्त कर आत्यन्तिक मुक्ति के अन्तहीन आनन्द का रसास्वादन करें!
चतुर्दश अध्याय
उपसंहार
मनुष्य अपनी दिव्य प्रकृति को विस्मृत कर चुका है। स्वार्थ, व्यसन तथा लोभ के कारण वह अधोगति को प्राप्त हो चुका है। प्रेम तथा घृणा के अन्तर्द्वन्द ने उसे पथ-भ्रान्त कर दिया है।
त्रिगुण-सापेक्ष यह संसार संघर्ष तथा कलह का युद्ध-क्षेत्र है। यहाँ शुभ-अशुभ, सुर-असुर तथा सत्त्व-तमस् में निरन्तर संघर्ष चल रहा है। अतः जन-संगठन वर्तमान युग की सर्वोपरि माँग बन गया है। संगठन में हमारी शक्ति निहित है। लोगों को अपने तुच्छ विवादों का परित्याग कर राष्ट्र तथा विश्व के शक्ति-संवर्धन के लिए मानसिक, हार्दिक तथा आत्मिक एकता के सूत्र में सम्बद्ध हो जाना चाहिए।
एकता : एक तात्कालिक आवश्यकता
मित्रो, आप सब शक्तिहीन हैं। आप लोगों में न एकता है, न संगठन। नदी के किनारे बिखरे हुए कंकड़ों की भाँति आप लोग भी बिखरे हुए हैं। यहाँ असंख्य उपजातियाँ एवं अगणित सम्प्रदाय तथा मत-मतान्तर हैं। देश की जन-संख्या में इनका बाहुल्य आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध नहीं होगा। अधिकांश लोग स्वार्थी हैं। उनमें सेवा तथा आत्म-बलिदान की भावना नहीं है। यह एक शोचनीय स्थिति है। संगठन से ही आपकी या किसी अन्य राष्ट्र की शक्ति तथा सुरक्षा सम्भव है।
मित्रो, आप लोग सिकता तथा पारद-कणों की भाँति इतस्ततः बिखरे हुए हैं। सम्बद्धता से ही आप लोगों को आत्म-रक्षा तथा देश के कल्याण के लिए समुचित शक्ति प्राप्त हो सकेगी। संगठन में आप लोगों का उत्थान तथा विभाजन में पतन निहित है। आँखें खोलिए और शैथिल्य, सम्मूढ़ता तथा उदासीनता का परित्याग कीजिए। संगठित हो कर कर्म करने के लिए आप लोगों का आह्वान हो रहा है। एक क्षण भी प्रतीक्षा मत कीजिए। उठिए और स्वावलम्बी हो जाइए।
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई-आप जो भी हों, अपने मत के प्रति निष्कपट भाव से आस्थावान् रहिए। अपनी आत्मा को प्रेमाप्ति से उद्दीप्त कीजिए। कटिबद्ध हो कर अपनी आत्मा में शक्ति का संचार कीजिए और एकात्म हो जाइए।
क्या आपको एक वृद्ध और उसके लकड़ियों के गट्ठर की कहानी याद है? उसके पुत्र उस पूरे गडर को तो तोड़ पाने में असमर्थ रहे; किन्तु एक-एक लकड़ी के उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। इसी प्रकार संगठित हो कर आप लोग भी शक्तिशाली और अजेय बन सकते हैं। आप लोगों में अपने कृत्य से लोगों को चमत्कृत कर देने की शक्ति है।
आप लोग अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए उद्यत हो जाइए। आप लोग अपनी वाणी और अपनी आकांक्षाओं में समस्वरता की सृष्टि कीजिए, एकता के सूत्र में पूर्णतः आबद्ध हो जाइए और अपने धर्म के प्रति स्वयं में अपरिचित प्रेम जाग्रत कीजिए। आपका हृदय प्रेम की ज्वाला से निरन्तर प्रोज्ज्वल रहना चाहिए। सबको अपना प्यार दीजिए। प्रेम से महान् कोई धर्म नहीं है।
धर्म की सेवा का सुयोग्य अधिकारी कौन है?
धर्म-सेवा के आकांक्षी जनों को साहस, दया, सरलता, सहिष्णुता, अनुकूलन की शक्ति, आत्म-निग्रह, विश्व-प्रेम, समदृष्टि, विनम्रता, मानसिक सन्तुलन, सत्य, धैर्य, शान्ति, क्षमा, आर्जव आदि गुणों से सम्पन्न होना चाहिए। उनके लिए इन गुणों को विकसित करते रहना आवश्यक है। उन्हें कर्मयोग का ज्ञान होना चाहिए। उनके लिए गीता के द्वितीय तथा तृतीय अध्याय का पुनः पुनः अध्ययन आवश्यक है। उनमें कर्म-फल की फलाशा नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने समस्त कर्म भगवान् को अर्पित कर देने चाहिए। उन्हें कर्तृत्व-भाव से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। उन्हें इस सत्य से सुपरिचित हो जाना चाहिए कि भगवान् ही उनके माध्यम से कर्म कर रहा है। तभी उनकी चित्त-शुद्धि सम्भव है। परमात्मा समाज का मूलाधार है। यह जगत् उसी पर अधिष्ठित है। उसके बिना कोई भी अणु गतिशील नहीं हो सकता। हमारी स्थिति, हमारी गति और हमारा अस्तित्व उसी पर निर्भर है। जो युवक अपना जीवन धर्म की सेवा में उत्सर्ग कर देना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अत्यावश्यक है। इसके फल-स्वरूप धर्म की सेवा समुचित विधि से हो सकेगी और युवक भी स्वार्थपरता से मुक्त रह सकेंगे। भगवान् को नूतन पुष्पों के साथ-साथ स्वस्थ, सबल तथा निष्कलुष शरीर एवं मन भी अर्पित करना चाहिए।
आप पूछ सकते हैं-"मुझे कर्मयोग तथा आत्म-निग्रह का अभ्यास क्यों करना चाहिए? मैं अपने अहंकार को विनष्ट क्यों करूँ? मैं स्वयं में त्याग तथा वैराग्य के भाव का विकास क्यों करूँ? मुझे मन को नियन्त्रित क्यों करना चाहिए?" इन प्रश्नों के उत्तर में मुझे यही कहना है कि इससे आपको स्वातन्त्र्य तथा पूर्णता की सम्प्राप्ति में योगदान प्राप्त होगा और आपको कष्ट, दुःख तथा मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होगी।
शिक्षा तथा राष्ट्र-निर्माण
हमारे सामने महान् आदर्श की सम्प्राप्ति का लक्ष्य है। किन्तु ऋषियों तथा सन्तों की पावन भूमि भारत आज भी अज्ञान के पंक से ग्रस्त है। जनसंख्या का अधिकांश निरक्षर है। प्राध्यापकों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को अवकाश के समय गाँवों में जा कर लोगों में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। इन्हें इनके लिए रात्रि-पाठशालाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्तियों को चाहिए कि वे इस कार्य मैं अधिकाधिक सहायता और सहयोग दें। अमेरिका तथा यूरोप से भारत की तुलना कीजिए। किसी भी सभ्य देश की अपेक्षा भारत में निरक्षरों की संख्या अधिक है।
आध्यात्मिक मूल्य : वास्तविक शिक्षा का आधार
युवकों तथा युवतियों के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना एक अनिवार्य आवश्यकता है। बालक-बालिकाओं के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय भावना को इसी विधि से जीवित रखा जा सकेगा। जो शिक्षा आपको सत्य तथा धर्माचरण के मार्ग पर अग्रसर करती है, जो आपके चरित्र के रूपान्तरण में समर्थ है, जो स्वातन्त्र्य, पूर्णता तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति में आपकी सहायिका सिद्ध होती है और इसके साथ ही जो आपको निष्कपट जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है, उसी को आदर्श शिक्षा कहा जा सकता है।
शरीर-विज्ञान का महत्त्व
देश के कोने-कोने में सेवा दलों, सभा-समितियों तथा व्यायामशालाओं की स्थापना होनी चाहिए। उनका संगठन समुचित विधि से होना चाहिए। इन संस्थाओं की अकृत्रिम सेवा आपका कर्तव्य है। इससे आपके अन्तर्गत निष्कलुष भावनाएँ विकसित होंगी और शीघ्र ही आपका हृदय विशुद्धता को प्राप्त हो जायेगा।
संसार को स्वस्थ माताओं तथा स्वस्थ बालक-बालिकाओं की आवश्यकता है। किन्तु, आजकल हम भारत में क्या देख रहे हैं? भारत-भूमि ने भीष्म, द्रोण, भीम, अर्जुन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम तथा असंख्य वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। यह भूमि अदम्य साहस, अद्वितीय शौर्य तथा अप्रतिम शक्ति से सम्पन्न अगणित राजपूत सामन्तों की जननी रही है; किन्तु आज यह ऐसे नपुंसकों का वास-स्थान बन कर रह गयी है जो अपने भरण-पोषण के लिए शत-शत बाह्य तत्त्वों के मुखापेक्षी हैं। इन लोगों को कतिपय उन वीर नायकों एवं मेधावी महापुरुषों का अनुकरण करना चाहिए जो आज भी भारत की मुकुटमणि हैं। भारत को नैतिक तथा आध्यात्मिक गुणों से सम्पन्न ऐसे असंख्य वीर सैनिकों की आवश्यकता है जिनमें पंच-सद्गुण-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह-विद्यमान हैं। जो लोग उक्त गुणों से सम्पन्न होने के साथ-साथ स्वस्थ, सबल तथा आत्मविद् है, वही लोग सब लोगों की वास्तविक स्वतन्त्रता की सुरक्षा में समर्थ हो सकते हैं।
बाल-विवाह : एक सामाजिक अभिशाप
बाल-विवाह एक महान् सामाजिक अभिशाप है। इसके परिणाम-स्वरूप बालक ही बालक का पिता बन जाता है। फलतः भारत कृशकाय व्यक्तियों का देश हो गया है। जीवन-यापन की उच्चतर विधियों से अभिज्ञ हो कर बाल-विवाह की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए।
कर्तव्य तथा अनुशासन पर बल की आवश्यकता
भौतिक शरीर संसार का सर्वाधिक आश्चर्यप्रद यन्त्र है। इसका संगठन विभिन्न प्रणालियों तथा अवयवों द्वारा हुआ है। इन प्रणालियों तथा अवयवों की समस्वरता एवं सम्पुष्टि पर ही आपका उत्तम स्वास्थ्य अवलम्बित है। यदि इनमें से एक भी प्रणाली या एक भी अवयव विकृत हो जाता है, तो असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आप रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक दुश्चक्र की सृष्टि हो जाती है। इसी प्रकार एक समाज या राष्ट्र का निर्माण विभिन्न समुदायों तथा व्यक्तियों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन समुचित विधि से करना चाहिए। अपने कर्तव्य-पालन के लिए उसका स्वस्थ तथा सबल होना नितान्त आवश्यक है। इसके अभाव में समाज या राष्ट्र शक्तिहीन हो कर पतन और अधोगति को प्राप्त हो जायेगा।
केवल किशोर-सुलभ उत्साह से कुछ नहीं होगा। इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति असम्भव है। आप लोगों में अकृत्रिम प्रेम की प्राण-प्रतिष्ठा अत्यावश्यक है। आपकी नस-नस में विशुद्ध प्रेम का स्पन्दन होना चाहिए। यदि आपमें इस प्रवृत्ति का अभाव है, तो आपको इसे मानवता की सेवा के माध्यम से चरम सीमा तक विकसित करना होगा। आपको उन महान् साधु-सन्तों के जीवन-चरित्र का पुनः पुनः अध्ययन करना चाहिए जिन्होंने धर्म के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। आप कुछ दिनों के लिए किसी आचार्य की शरण में जाइए। वहाँ रह कर आप उनका आदर-सत्कार तथा आदेश-पालन कीजिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति नेता बन कर नेतृत्व-ग्रहण करना चाहेगा, तो आन्दोलन समाप्त हो जायेगा। सेवा तथा आज्ञा-पालन के माध्यम से आप धर्म और समाज की सेवा सम्यक् विधि से कर सकेंगे।
औद्योगिक विकास तथा आर्थिक स्वावलम्बन
स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर औद्योगिक विकास का पथ प्रशस्त कीजिए। इससे हमें आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी जो हमारे लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
विवाहोत्सव तथा अन्य समारोहों में धन का अपव्यय किया जाता है। इस धन को बचा कर इसका उपयोग राष्ट्र-निर्माण में कीजिए। इस दिशा में हुए एक-एक पैसे के उपयोग को समुचित व्यय कहा जायेगा। सामाजिक रूढ़ियों का दास मत बनिए। ये प्रगति के मार्ग में अवरोध उपस्थित करती हैं जिससे राष्ट्र शक्तिहीन होता है।
हमारे युवा स्नातकों को उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र को नगण्य नहीं समझना चाहिए। उन्हें अपनी कृषि की देख-रेख करते हुए इसकी उत्पादन-शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। इस दिशा में करने को बहुत कुछ है। इससे वे स्वतन्त्र रूप से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोगों को स्वास्थ्यवर्धक विशुद्ध दूध-मक्खन तथा खाद्यान्न की आपूर्ति कर पर्याप्त मात्रा में धनोपार्जन भी कर सकते हैं।
श्रमसाध्य सक्रिय जीवन तथा सहन-शक्ति से निःसृत होने वाली शक्ति
धैर्यशील बनिए। दृढ़तापूर्वक श्रम में संलग्न हो जाइए। कुछ ऐसा करते रहिए जो व्यावहारिक हो। सफलता का रहस्य इसी में निहित है। अर्थहीन प्रलाप से कोई लाभ नहीं। प्रत्येक शुभ विचार क्रियान्वित कर दीजिए। मंच पर भाषण दे देने मात्र से क्षणिक भावावेश तथा अर्थहीन उत्साह के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ नहीं आयेगा। इस प्रकार का अभियान अधिक लाभप्रद नहीं होता। वस्तुओं को सम्यक् विधि से संयोजित कीजिए।
जीवन में सहनशीलता को स्थान दीजिए; अपमान, अभाव तथा कष्ट सहन कीजिए; वस्त्र-प्रक्षालन कीजिए; लकड़ियाँ काटिए तथा पानी लाया कीजिए। शारीरिक श्रम आवश्यक है। अपने शरीर तथा इसकी मांस-पेशियों को सुदृढ़ बनाइए, दण्ड-बैठक कीजिए. मल्लयुद्ध तथा आसन-प्राणायाम कीजिए, मुक्त वायु में दौड़ लगाइए और शारीरिक शक्ति तथा स्वास्थ्य की रक्षा करते रहिए। सरल तथा नैसर्गिक जीवन-यापन कीजिए, वीर्य की रक्षा कीजिए, विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए और इन्द्रिय-निग्रह का पाठ पढ़िए।
विलास तथा ऐहिक सुख अभिशाप हैं। इनसे आपकी शक्ति क्षीण होगी। प्रतिदिन तीन या चार मील दौड़ लगाइए। युवा पीढ़ी की दशा शोचनीय है। वे आधा मील भी नहीं दौड़ सकते। उनका स्वास्थ्य सन्तोषजनक नहीं है। वे रक्ताभाव, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता, दौर्बल्य आदि रोगों से प्रस्त हैं। विपत्ति के समय वे अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। वे शक्तिहीन, भीरु तथा पुंसत्वहीन हो चुके हैं। क्या यह स्थिति शोचनीय नहीं है?
अपने उत्तरदायित्व को समझिए। कष्ट तथा कठिनाइयों से जूझते हुए सुदृढ़ रह कर जीवन-यापन कीजिए। साहसी तथा प्रसन्नचित्त बने रहिए। अमर्त्य आत्मा के नियमित ध्यान के माध्यम से अपने अन्तर्तम से शक्ति तथा साहस प्राप्त कीजिए। एकान्त में बैठ कर कुछ समय के लिए अपने भीतर झाँकिए। विलास तथा अकर्मण्यता को तिलांजलि दे डालिए। कठोर श्रम कीजिए और विजय-माला धारण कर बाहर आइए। महान् पुरुषों ने धर्म की रक्षा तथा सन्मार्ग पर अविचलित बने रहने के लिए अनेक कष्ट सहन किये हैं। हमारे हृदय में वे आज भी जीवित हैं। उनका महिमा-मण्डित जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।
राष्ट्र के संगठन के लिए आह्वान
मेरे सिख बन्धुओ! आप लोग शूरवीर योद्धा और साहसी हैं। आप लोगों की नसों में गुरु गोविन्दसिंह का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आप लोग शक्तिमान् तथा हृष्ट-पुष्ट शरीर के स्वामी हैं। यह सब प्रभु की कृपा का फल है। आप सब हमारे राष्ट्र के क्षत्रिय हैं।
हिन्दुओ, सिखो, मराठो तथा राजपूतो! जिस प्रकार अथाह अन्ध महासागर में असंख्य रत्न गर्भित हैं, उसी प्रकार आप लोगों में भी अनेक रत्न छिपे हैं। आप लोगों में अनेक रणजीतसिंह, अनेक शिवाजी और अनेक राणाप्रताप हैं। अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जाग्रत कीजिए और अपने पूर्वजों की शक्ति तथा उनके गौरव का स्मरण करते हुए आगे बढ़िए। अपने स्वभावगत शौर्य तथा अदम्य उत्साह का प्रदर्शन कीजिए और समग्र राष्ट्र के संगठन में संलग्न हो जाइए।
साधु-संन्यासियों से निवेदन
सिद्ध साधुओ, संन्यासियो, योगियो तथा ब्रह्मचारियो! आप लोगों से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि आप लोग अपने एकान्त आश्रमों से बाहर आ कर मानवता की सेवा कीजिए। आप लोगों को किसी भी आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को वही करना है जो समर्थ रामदास ने किया था। रामदास शिवाजी को सम्यक् परामर्श दिया करते थे। शिवाजी अपने गुरु से प्रेरणा ग्रहण करते थे। उन्होंने गैरिक ध्वज फहराते हुए बहुत कुछ कर दिखाया। रामदास की उपस्थिति शिवाजी के लिए प्रेरणा-स्रोत थी। इसी प्रकार आप लोग भी लोगों को नैतिक उपदेश तथा सत्परामर्श दे सकते हैं। आप लोग उनका पथ-प्रदर्शन तथा उन्हें अपने प्रवचनों से प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप लोग वैसा सभी कुछ कर पाने में समर्थ हैं जो राष्ट्रीय एकता के हित में सर्वाधिक उपयोगी है। किसी के साथ आप लोगों का रागात्मक सम्बन्ध नहीं है और आप लोग आध्यात्मिक शक्ति से सम्पन्न हैं। अतः आप लोग अपने कर्म से लोगों को चमत्कृत कर सकते हैं। आप लोग अपने प्रवचनों में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की बात किया करते हैं। आप लोग इसे कार्य-रूप में परिणत करने की कृपा कीजिए और वेदान्त को व्यवहार-भूमि पर उतारिए। धर्म सर्वदा के लिए सुरक्षित रहे! सभी नागरिक विशुद्ध प्रेम के बन्धन में आबद्ध हो कर संगठित हों! देश के कल्याण तथा उसकी सुदृढ़ता के लिए आप सब मिल कर काम करें! सभी लोग आध्यात्मिक एवं भौतिक दृष्टि से महिमान्वित तथा समृद्ध हों!
ॐ शान्ति ! शान्ति ! शान्ति !
परिशिष्ट-१
शिव-लिंग
(एक प्रतीक जो किसी अनुमिति की ओर संकेत करता है)
विदेशियों में यह धारणा सामान्य रूप से व्याप्त है कि शिव-लिंग जननेन्द्रिय एवं प्रजनन-शक्ति अथवा सन्तति-प्रवाह-सम्बन्धी प्राकृतिक सिद्धान्त का द्योतक है; किन्तु यह एक शोचनीय तथा सामान्य भूल न हो कर एक अत्यधिक भ्रान्तिपूर्ण अवधारणा है। उत्तर वैदिक काल में लिंग भगवान् शिव की प्रजनन-शक्ति का प्रतीक बन गया। लिंग एक विशिष्ट चिह्न है। यह असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि यह काम से सम्बद्ध कोई चिह्न नहीं है।
लिंगपुराण में आया है :
प्रधानं प्रकृतिं तच्च यदाहुर्लिंगमुत्तमम् ।
गन्ध-वर्ण-रसैहींनं शब्द-स्पर्शादि-वर्जितम्।
"अग्रवर्ती लिंग जो आद्य एवं गन्ध-वर्ण-रस-स्पर्श-रहित है, उसको प्रकृति कहा जाता है।"
संस्कृत में लिंग को चिह्न कहते हैं। यह एक ऐसा प्रतीक है जो किसी अनुमिति की ओर संकेत करता है। जब आप नदी में भयंकर बाढ़ देखते हैं, तब आप अनुमान कर लेते हैं कि पिछले दिन मूसलाधार वर्षा हुई है और जब आपको धूम दृष्टिगत होता है, तब वहाँ आपको अग्नि का अनुमान होता है। अनेक रूपों से समन्वित यह विराट् विश्व सर्वव्यापी भगवान् का लिंग है। शिव-लिंग भगवान् शिव का प्रतीक है। लिंग-दर्शन के समय आपका मन तत्क्षण ऊर्ध्वमुखी हो जाता है और आप भगवच्चिन्तन में लीन हो जाते हैं।
भगवान् शिव निश्चित रूप से निराकार हैं। उनका अपना कोई रूप नहीं है; अपितु सभी रूप उन्हीं के रूप हैं। वे सभी रूपों में व्याप्त हैं। सभी रूप भगवान् शिव का रूप अर्थात् उनका लिंग हैं।
मन की एकाग्रता का एक सशक्त माध्यम
मन की एकाग्रता के लिए लिंग में एक रहस्यमयी अर्थात् अवर्णनीय शक्ति है। जिस प्रकार मन स्फटिक-मणि पर सरलतापूर्वक केन्द्रित हो जाता है, उसी प्रकार लिंग-दर्शन से मन एकाग्र हो जाता है। यही कारण है कि भारत के प्राचीन ऋषियों तथा द्रष्टा मनीषियों ने शिव-मन्दिर में लिंग की प्राण-प्रतिष्ठा के निर्देश दिये थे।
लिंग निराकार शिव का प्रतीक
शिव-लिंग आपसे मौन की निर्भान्त भाषा में वार्तालाप करता है- "मैं अद्य एवं निराकार हूँ।" इस भाषा को विशुद्ध-हृदय जन ही समझ सकते हैं। एक कौतूहल-प्रिय, दुर्भाव-प्रवण, अपवित्र तथा अल्पज्ञ विदेशी व्यंगात्मक स्वरों में प्रलाप करता है- "ओ! ये हिन्दू जननेन्द्रिय का पूजन करते हैं। ये लोग अज्ञानी हैं और इनका कोई दर्शन-शास्त्र नहीं है।" जब कोई विदेशी तमिल या हिन्दी भाषा सीखने का प्रयत्न करता है, तब वह सर्वप्रथम कुछ अश्लील अशोभन शब्दों का ही चयन करता है। यही उनकी कौतूहलमयी प्रकृति है। इसी प्रकार कुछ कौतूहल-प्रिय विदेशी प्रतीकोपासना में मीन-मेख निकालने लगते हैं। लिंग निराकार सत्ता भगवान् शिव का केवल बाह्य प्रतीक मात्र है जो अविभाज्य, सर्वव्यापी, शाश्वत, शुभ, नित्य शुद्ध तथा इस विराट् विश्व के अमर्त्य सारतत्त्व हैं और जो आपके अन्तर्यामी, अन्तर्तम आत्मा एवं सर्वोच्च ब्रह्म से अभिन्न हैं।
स्फटिक-लिंग : निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक
स्फटिक-लिंग भी भगवान् शिव का प्रतीक है। भगवान् शिव के आराधन-पूजन के लिए इसे उपयुक्त माना गया है। यह स्फटिक-मणि से निर्मित होता है। यह स्वयं वर्णहीन होता है; किन्तु यह जिस किसी भी वस्तु के सम्पर्क में आता है, उसी का वर्ण ग्रहण कर लेता है। यह निर्गुण तथा अलक्षण आत्मा अर्थात् निराकार तथा निर्गुण शिव का द्योतक है।
शिला-खण्ड में निहित रहस्यमयी शक्ति
किसी निष्कपट भक्त के लिए लिंग एक शिला-खण्ड न हो कर एक प्रदीप्त तैजस् तथा चेतन तत्त्व है। वह उसके साथ वार्तालाप करता, उसके नेत्रों को भावाश्रु-पूरित करता और उसके मन को रोमांचित करता है। इससे उसका हृदय द्रवित हो उठता है और वह उसकी सहायता से देहाध्यास से ऊध्र्वोन्मुख हो कर भगवान् से तादात्म्य स्थापित कर लेता है जिसके फल-स्वरूप उसे निर्विकल्प-समाधि की प्राप्ति हो जाती है। भगवान् राम ने रामेश्वरम् में शिव-लिंग का पूजन किया था और महापण्डित रावण ने स्वर्ण-निर्मित शिव-लिंग की पूजा की थी। इस लिंग में कितनी रहस्यमयी शक्ति निहित है!
जो भगवान् शिव का प्रतीक है, जो मन की एकाग्रता में सहायक सिद्ध होता है और जो प्रारम्भ में नव-दीक्षितों के मन के आलम्बन के लिए एक साधन का उत्तरदायित्व वहन करता है, उस लिंग के पूजन के माध्यम से आपको निराकार शिव की प्राप्ति हो!
परिशिष्ट-२
भगवद्गीता : भारतीय संस्कृति की आधारशिला
अनासक्ति का उपदेशामृत
आध्यात्मिक मूल्य तथा जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण सम्यक् संस्कृति की आधारशिला हैं। मानव की मूलभूत दिव्य चेतना के प्रति आग्रहशीलता भारतीय संस्कृति का सारतत्त्व है। भारतीय सभ्यता आन्तरिक विशुद्धि तथा मनुष्य में अन्तर्निहित आध्यात्मिक प्रकाश पर अधिष्ठित है। भारत अध्यात्म की भूमि है और प्रत्येक सच्चा भारतीय आत्म-स्वराज्य अर्थात् आन्तरिक एवं बाह्य प्रकृति पर विजय द्वारा उपलब्ध आत्मा की सर्वोच्च दिव्यता में निहित स्वातन्त्र्य का अभीप्सु है। भारतीयों का अन्तिम प्राप्तव्य आत्म-साक्षात्कार है। भगवद्गीता एक सार्वजनीन धर्मग्रन्थ एवं भारतीय परम्परा की समीचीन तथा सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। गीता अनासक्ति, आत्मा के अमरत्व तथा निरपेक्ष सत्ता में आत्मा के स्वातन्त्र्य का धर्मोपदेश है। यह आत्म-तत्त्व की सर्वग्राही आन्तरिकता का पावन प्रशिक्षण है। अनासक्ति की अपरिहार्यता ब्रह्माण्डीय एकत्व के बोध की अनुवर्तिनी है। श्रीकृष्ण की साधिकार उद्घोषणा के अनुसार उनके अतिरिक्त विश्व में अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है (७-७)। सत्य जीवन की अविभाज्यता में निहित है। अतः नाम-रूपों के प्रति आसक्ति मिथ्या के प्रति आकर्षण तथा सत्य का समतिक्रम है जिसका अपरिहार्य परिणाम दुःख है। गीता (५-२२) में भगवान् कहते हैं कि इन्द्रियों तथा विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न जो भोग हैं, वे दुःख के कारण हैं। अनासक्ति सम्यक् वैराग्य की भावना तथा शुभ कर्म की द्योतक है जो कर्ता को फलाशा से मुक्त कर देती है। सम्यक् संस्कृति हमें स्वतन्त्रता की ओर अभिमुख करती है और यह भारतीय द्रष्टश ऋषियों के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने अपनी गहन प्रज्ञा-शक्ति द्वारा मनुष्य में अन्तर्निहित शाश्वत आत्मा के स्वातन्त्र्य का साक्षात्कार कर लिया था तथा सम्पूर्ण जगत् के समक्ष इस सत्य की उद्घोषणा भी कर दी थी।
निस्पृहता तथा आन्तरिक शान्ति भारतीय संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं। जिस ज्ञान से सम्यक् संस्कृति को अभिलक्षित किया जाता है, वह शाब्दिक पाण्डित्य न हो कर नैतिक पृष्ठभूमि पर अधिष्ठित विशुद्ध प्रज्ञा है। किसी व्यक्ति के नैतिक अनुशासन के मापदण्ड से ही उसके ज्ञान का मूल्य निर्धारण किया जाता है। ज्ञान का पर्यवसाय सामान्य ज्ञान में न हो कर जीवन के गहनतम सत्य के साक्षात्कार में होता है। पूर्वाग्रहहीनता एवं कायिक तथा वैचारिक अनासक्ति के अभाव में इस प्रकार का सुसंस्कृत जीवन असम्भव है। गीता (३-२५) में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं, "जिस प्रकार कर्मों में आसक्त अज्ञानी जन कर्म करते हैं, उसी प्रकार तत्त्ववेत्ता विद्वान् पुरुष को भी लोक-संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए।" जागतिक वस्तुओं के साथ सामान्य एवं सतत सम्पर्क के कारण मनुष्य उनसे रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए विवश हो जाता है; किन्तु ये वस्तुएँ तत्त्वतः मिथ्या होती हैं और इनके मिथ्या स्वरूप की अभिज्ञता के अभाव में पूर्ण अनासक्ति असम्भव है। भारतीय मनीषा ने मन तथा इन्द्रियों के आदेशों के सम्मुख नतमस्तक होने वाले व्यक्तियों द्वारा मान्य जीवन के प्रति गर्हित दृष्टिकोण में निहित भ्रान्तियों को अनावृत कर विषयात्मक ऐहिक जीवन की क्षणभंगुरता के तथ्य को सुस्पष्ट किया था। दुःख तथा क्लेश की अनुभूति एवं ऐन्द्रिक जगत् में जीवन की अपर्याप्तता सभी दर्शनों का प्रारम्भ बिन्दु हैं। विवेकशील पुरुष में भौतिक जीवन के बन्धनों से मुक्ति की कामना विद्यमान रहती है। वह नश्वर वस्तुओं के प्रति आस्थावान् नहीं होता। गीता के अनुसार यह संसार 'अनित्यम्', 'असुखम्', 'दुःखालयम्' तथा 'अशाश्वतम्' है। जब किसी व्यक्ति में यह विवेक जाग्रत होता है, तब वह निस्पृह हो जाता है और किसी वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रह जाती। अन्तरतः ईश्वरमय हो जाने के कारण बहिरंग जीवन की क्षुद्रता अनावृत हो जाती है और तब पूर्णता का वह अन्वेषी अनित्य प्रतीतियों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भारतीय संस्कृति धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना की शक्ति की समृद्धि का पर्याय है जिसके अभाव में मनुष्य उस पशु की अपेक्षा कुछ ही अधिक श्रेष्ठतर होता है जिसमें केवल नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ ही विद्यमान हैं। गीता बाह्य रूपों के प्रति आस्था तथा इनकी आकांक्षा के परित्याग का उपदेश और इस बात पर बल देती है कि जो व्यक्ति शाश्वत शान्ति के प्रति आग्रहशील है, उसके विचार तथा कर्म में स्वार्थपरता और किसी विशेष भौतिक लक्ष्य की सम्प्राप्ति के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गीता (२-४८) में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं- "तुम योग में स्थित हो कर अनासक्त भाव से कर्म करो।" गीता की आग्रहशीलता इस तथ्य के प्रति है कि निस्संग तथा ईश्वर में लीन रहते हुए कर्म करते रहना सम्यक् जीवन-यापन की कला एवं इहलोक तथा परलोक में शान्ति-प्राप्ति का उत्तम साधन है। इस लक्ष्य की सम्प्राप्ति के लिए किये गये प्रत्येक प्रयत्न का फल अनश्वर होता है। गीता (२-४०) में श्रीकृष्ण कहते हैं-"इसमें न तो अभिक्रम का नाश होता है, न इससे किसी प्रत्यवाय दोष की उत्पत्ति होती है। इस धर्म का अत्यल्प अनुष्ठान भी महान् भय से रक्षा करता है।" इस दिशा में किया गया कोई भी प्रयत्न व्यर्थ नहीं होता। प्रत्येक प्रयत्न से उनके अनुरूप फल की सिद्धि हो जाती है; क्योंकि आत्मा अपने तात्त्विक स्वरूप में नित्य है।
आत्मा का अमरत्व
भारतीय जिस महान् सत्य के प्रति आस्थावान् हैं और जो उनके लिए अविस्मरणीय तथा विश्वसनीय है, वह है आत्मा का अमरत्व तथा जीवन का सतत प्रवाह। गीता (२/१७-१८) प्रारम्भ में ही कहती है- "यह सब-कुछ जिससे व्याप्त है, उसे तू अविनाशी जान। उस अव्यय के विनाश में कोई भी समर्थ नहीं है। वह अज तथा अमर्त्य है। वह अभाव को नहीं प्राप्त होता। वह अज, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर-नाश के पश्चात् भी उसका नाश नहीं होता।" इस सर्वोच्च सत्य की अभिज्ञता से अधिक अन्य कोई भी वस्तु गौरवपूर्ण नहीं है। यह प्राणदायक ज्ञान भारतीयों की राष्ट्रीय संजीवनी शक्ति, मानव-जाति के लिए सान्त्वना तथा श्रीकृष्ण के रूप में निरपेक्ष ब्रह्म द्वारा मानवता के साक्षात् प्रतिनिधि अर्जुन को दिया गया उपदेश है। भारतीय संस्कृति मनुष्य में अन्तर्निहित आत्मा की अनश्वरता एवं दिव्यता के प्रति असन्दिग्ध आस्था से पूर्णतः प्रभावित एवं सर्वांगतः परिव्याप्त है। हिन्दुओं के लिए इन्द्रिय-जन्य अनुभवों का संसार यथार्थ नहीं है। उनके लिए जो यथार्थ है, वह है ब्रह्म या आत्मा। उनका पूर्ण विश्वास स्थैर्यहीन जगत् के प्रति न हो कर शाश्वत सत्ता के प्रति है। ईश्वर ही उनका लक्ष्य है और संसार इस लक्ष्य-सिद्धि का एक मार्ग या साधन मात्र है। यह उनके अनुभवों की इतिश्री नहीं है। गीता उस अनुभवातीत जीवन का सन्देश है जिसमें सम्पूर्ण जगत् समाहित है जो एक अभिनव प्रकाश में दृष्टिगत होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस अनुभव का अधिकारी है। दुष्ट तथा पापी जन के लिए भी इसके द्वार मुक्त हैं। गीता (९/३०-३२) में भगवान् कृष्ण कहते हैं- "यदि कोई अतिशय कुत्सित आचरण वाला मनुष्य भी मुझे अनन्य भाव से भजता है, तो उसे भी साधु ही समझना चाहिए; क्योंकि वह यथार्थतः निश्चययुक्त हो चुका होता है। जो पाप-योनि वाले हैं, वे भी मेरी शरण में आ कर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं।" मनुष्य में आद्य या अन्तर्जात पाप जैसी कोई वस्तु नहीं है; क्योंकि आत्मा अमर्त्य है और "जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में काष्ठ-समूह भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं" (गीता : ४-३७) । यहाँ ज्ञान से तात्पर्य अव्यय आत्मा के साक्षात्कार से है। मनुष्य अपनी इच्छाओं तथा अपने कर्मों के अनुसार एक जन्म से दूसरे जन्म तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में उस समय तक संक्रमण करता रहता है, जब तक वह अपनी इच्छाओं तथा अपने कर्म से उद्भूत संस्कारों को नष्ट कर ईश्वर से तादात्म्य-लाभ नहीं कर लेता। इसका कारण यह है कि ईश्वर से एकात्मता ही मनुष्य की नियति है। जब तक आत्म-साक्षात्कार के प्रसाद की सम्प्राप्ति नहीं हो पाती, तब तक पुनर्जन्म की प्रक्रिया में कोई अन्तराय नहीं उपस्थित हो सकता; क्योंकि अमर्त्य आत्मा आत्म-साक्षात्कार के लिए प्रति क्षण निश्चयात्मक रूप से आग्रहशील रहा करता है। आत्म-साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु से मनुष्य को शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती और जब तक सारे कर्म ज्ञानामि में दग्ध या निर्बीज नहीं हो जाते, तब तक आत्म-साक्षात्कार असम्भव है। पुनर्जन्म तथा आत्मा के अमरत्व का हिन्दू-सिद्धान्त विश्व के धार्मिक इतिहास में एक अद्वितीय सिद्धान्त और जीवन की अर्थवत्ता की एकमात्र वैज्ञानिक तथा सन्तोषप्रद व्याख्या है। अमर्त्य आत्मा के प्रति मूलभूत सहमति के अभाव में किसी भी अनुभव का बोध या इसकी मीमांसा सम्भव नहीं है। कर्म का सिद्धान्त तो उस मूलभूत सिद्धान्त का एक उप-सिद्धान्त मात्र है जो दर्शन तथा धर्म का केन्द्रस्थ तत्त्व तथा कथ्य है।
सामाजिक जीवन का आदर्श
दिव्य सत्ता के साथ जीवन की एकात्मता के प्रकाश में मनुष्य को अपने बातावरण के प्रति अनुकूलन की विद्या अपनानी पड़ती है। मनुष्यों के जीवन-स्तर में पारस्परिक वैभिन्य के दर्शन होते हैं और उनके धर्म तथा आचरण उनके वैयक्तिक विकास के इन्हीं स्तरों पर अधिष्ठित होते हैं। गीता व्यक्तियों के स्वभावगत वैषम्य तथा तज्जनित कर्तव्यों के वर्गीकरण के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करती है। उनके ये विभिन्न कर्म उनके विकासगत स्तरों के अनुरूप होते हैं जिनसे उनके कर्मों का निर्धारण होता है। सभी देशों में दार्शनिक, आध्यात्मिक, क्रियात्मक, युयुत्सु एवं व्यावसायिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। इनके अतिरिक्त दैनिक पारश्रमिक से जीविकोपार्जन करने वाले और शारीरिक कर्म में रुचि रखने वाले कुछ सामान्य जन भी रहते हैं। इस पृथक्करण की सृष्टि किसी अभिवृत्ति-विशेष से उत्प्रेरित हो कर कृत्रिम रूप से नहीं हुई है। वस्तुतः यह मनुष्य की आन्तरिक अभिव्यक्तियों के अनावरण के माध्यम से बाह्य सामाजिक व्यवस्था को निरूपित करती है। मनुष्य विकास के जिस चरण में पहुँच चुका होता है, उसी के अनुरूप उसके 'स्वधर्म' या कर्तव्य का निर्धारण होता है। उसकी इस स्थिति का उत्तरदायित्व अन्य लोगों पर न हो कर स्वयं उसी के आन्तरिक तथा स्वभावगत वैशिष्ट्य पर होता है जिसे वह अपने दैनन्दिन आचरण तथा कर्म के माध्यम से अभिव्यक्त किया करता है। चतुर्विध सामाजिक वर्गीकरण का उद्देश्य उन सभी लोगों में सुखद एवं मधुर सम्बन्ध को सुनिश्चित करना है जो अपनी अन्तर्निष्ठ प्रवृत्तियों के कारण अपनी क्षमता का प्रदर्शन पृथक् पृथक् अध्यवसायों में किया करते हैं और जिनके विचार तथा कर्म में साम्य के दर्शन नहीं होते। लोगों में विचार तथा कर्म की सादृश्यता असम्भव है। मानव-जीवन के अन्तरतम में इस प्रकार के साम्य का रेखांकन हुआ ही नहीं है। जीवन प्राणियों के पृथक् पृथक् जातिगत समूहों का प्रदर्शन-कक्ष है और व्यक्तियों का चतुर्विध वर्गीकरण ज्ञान तथा कर्म के लिए मानसिक विन्यास तथा क्षमता का एक बृहद् विभाजन है। सामाजिक कल्याण समाज के समुचित नियमन पर निर्भर करता है; किन्तु यह शासक की शक्ति के माध्यम से न हो कर उसके पद के विवेकपूर्ण बोध के माध्यम से होना चाहिए। उसे इस प्रक्रिया में स्वयं को अपने उस विशिष्ट पद के अनुरूप ढालना चाहिए जो स्वयं उसी के लिए सृजित किया गया है और जो उसके स्वभाव का नियमन करने वाले आन्तरिक विधान के अनुरूप है। समाज के सदस्य परस्पराश्रित होते हैं। उनका कल्याण उनके गुण-कर्म के अनुरूप सामाजिक वर्गीकरण से ही सम्भव है। भारत की पुरातन संस्कृति के परिरक्षण का श्रेय प्राकृतिक विधान एवं मनुष्य की आन्तरिक प्रकृति की उत्प्रेरणा पर अधिष्ठित इस विवेकपूर्ण परियोजना को ही है।
निस्सन्देह गीता सामाजिक एवं विश्वजनीन बन्धुत्व के आदर्श का प्रतिपादक एवं महान् ग्रन्थ है। फिर भी इस सम्बन्ध में उसके संकेतानुसार व्यक्तिगत जीवन, पारस्परिक जीवन, सामाजिक जीवन, वैश्विक जीवन तथा दिव्य जीवन को अन्ततः एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। ये केवल दिव्य पूर्णता के बोध की ओर अग्रसर व्यक्ति के विकास के विभिन्न चरणों के द्योतक हैं। एकात्मकता की आधार-भूमि पर अधिष्ठित होने के पश्चात् ही बन्धुत्व की सार्थकता की सिद्धि सम्भव है। समाज के कल्याण का निर्धारण धर्म द्वारा होता है और विश्व मानव जाति का एक बृहदू समाज है जिसमें इसके भिन्न-भिन्न अंग समाविष्ट हैं। सामाजिक कल्याण के अन्वेषी के लिए इस तथ्य का विस्मरण असम्भव है कि समाज विश्व में ही अवस्थित है जो एक समग्र इकाई और व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक विधान की सम्पुष्टि है। यह विश्व भी अपने-आपमें कोई स्वयं-विवृत सत्य न हो कर सर्वोच्च दिव्य सत्ता में अन्तर्निहित सामंजस्य तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति है। गीता (१३-३०) में भगवान् कृष्ण कहते हैं- "जब कोई भूतों के पृथक् पृथक् भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही सम्पूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।" इस यथार्थ सत्य का धर्म वह मानदण्ड है जिससे विश्व, समाज, परिवार तथा व्यक्ति के धर्म को निर्धारित किया जाता है। ब्रह्म की
वास्तविकता अगोचर है। अतः सार्वजनीन प्रेम एवं स्वार्थ तथा आसक्ति का परित्याग अखिल विश्व एवं इनके अवयवों का धर्म हो जाता है। सभी प्राणियों से निष्पक्ष तथा विरासक्त भाव से प्रेम करना चाहिए; क्योंकि सर्वभूतों की सत्ता इस निरपेक्ष आत्मा में ही निहित है। गीता में, विशेषतः इसके तेरहवें तथा सोलहवें अध्यायों में जिन ग्रहणीय गुणों की परिगणना की गयी है, वे व्यक्ति तथा समाज-दोनों के सुखद, कल्याणकर, श्रेयस्कर तथा आध्यात्मिक जीवन-यापन के लिए अनिवार्य हैं। दैवी-सम्पदा, नैतिक बल तथा आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति द्वारा मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियाँ पराभूत हो जाती हैं और अन्तर्भूत शाश्वत सिद्धान्त अनावृत हो उठता है। लोक-संग्रह अर्थात् विश्व का कल्याण तथा इसकी सुदृढ़ता गीता के सामाजिक नीति-शास्त्र का आदर्श है। अनासक्ति तथा आत्म-समर्पण की भावना और निर्विकार आत्मा के स्वभाव के ज्ञान से उत्प्रेरित हो कर स्वधर्म के पालन से इसका आचरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव है। सर्वभूत-हित स्वधर्म का लक्ष्य है। समाज के तन्तु-विन्यास का प्रयोजन इसके सदस्यों को जीवन के सर्वोच्च आदर्श के बोध में सहयोग प्रदान करना है। जीवन एक समग्र इकाई है और इसमें सभी प्राणियों की साझेदारी है जो इसके अवयव हैं। अतः इस जीवन के साथ उनकी समस्वरता पर ही उनका विकास निर्भर है। अवयव की पूर्णता समग्रता का एकत्व है। पारस्परिक प्रेम तथा समग्र के प्रति निष्ठापूर्वक कर्तव्य-पालन से व्यक्ति और समाज, दोनों कृतकृत्य होते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति बिना अरुचि एवं आसक्ति के अपना कर्तव्य पालन करता है, तब समाज का कल्याण सुनिश्चित हो जाता है; क्योंकि जहाँ कर्म का तादात्म्य इस दृश्यमान जगत् के मूल में निहित दैवी प्रयोजन के ज्ञान से होता है वहाँ श्री, विजय, विभूति तथा अविचल नीति का प्रादुर्भाव होता है (गीता : १८-७८)। गीता के अनुसार मानवीय आचरण के शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रों के माध्यम से ही हम इस सत्य से परिचित हो पाते हैं कि समाज शाश्वत सिद्धान्तों तथा आध्यात्मिकता के आधार पर ही अवलम्बित है।
मूलतः जीवन एक उपासना है। इस संसार में कर्म यथार्थतः विराट् ईश्वर के विश्व-रूप की पूजा है। मनुष्य दैवी विधान के निष्पादन का निमित्त अर्थात् माध्यम मात्र है। जीवन एक यज्ञ या पवित्र आत्माहुति है और संसार जो धर्मक्षेत्र है, वह वेदी है जिस पर मनुष्य स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है। धर्म व्यक्ति का नियमन करने वाला आचारगत मूल्य है। वह उसे मोक्ष के लिए उत्प्रेरित करता रहता है और मोक्ष 'अपरिमेय मूल्य' तथा जीवन का लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का अनुमोदन करना चाहिए जो जीवन का रक्षक है। धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो अनासक्ति या निष्काम आचरण द्वारा स्वयं उसकी रक्षा करता है। ईश्वर स्वयं 'शाश्वत धर्म-गोप्ता' अर्थात् सनातन धर्म का रक्षक है। धर्म भौतिक तथा आध्यात्मिक मंगल का मूल स्रोत है। धर्म का अनुपालन अर्थ, काम तथा मोक्ष का अधिष्ठान है। ईश्वर का साक्षात्कार सभी लोगों का सर्वोच्च धर्म है। अन्य सभी धर्म उसके अनुवर्ती मात्र हैं। ईश्वर में इन सबके चरम एकत्व का साक्षात्कार सम्पूर्ण विश्व में करना चाहिए (६/२९-३०)। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईश्वर का एक जीवन्त सत्य है जो इसके बाह्याभ्यन्तर में परिव्याप्त है और जिसकी सादृश्यता में कोई भी वस्तु कभी सक्षम नहीं हो सकती (९/४-५)। इस निरपेक्ष आदर्श की सम्पुष्टि सभी विचारों एवं कर्मों से होनी चाहिए। जिसकी सम्प्राप्ति अन्यत्र न हो कर केवल ईश्वर से ही हो पाती है, इस सार्वजनीन एवं सर्वोच्च कल्याण के प्रति आत्म-समर्पण की श्रेष्ठ भावना से परिपूरित हो कर जीवन-यापन से ही समाज की सुरक्षा सम्भव है। इस लक्ष्य के विस्मरण से जीवन दुःखमय हो जाता है। दैवी सम्पदा, ज्ञान तथा सर्वोच्च चेतना पर अधिष्ठित जीवन दिव्य जीवन हो जाता है।
सुसंस्कृत व्यक्ति
सुसंस्कृत व्यक्ति का गीतोक्त आदर्श वह व्यक्ति है जो स्थितप्रज्ञ, भागवत अथवा गुणातीत है। वह संस्कृति के सुन्दर पुष्प का परिपक्व फल है। जो इन्द्रियों के आदेश का अनुपालन नहीं करता, जो मन में स्थित समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जो आत्मा से आत्मा में ही सन्तुष्ट रहता है, वह पूर्ण मानव है (२-५५)। जो राग-द्वेष से ऊपर उठ चुका होता है, आत्म-साक्षात्कार के कारण जिसकी कामनाएँ नष्ट हो चुकी होती हैं, जिसका दिन अज्ञानियों के लिए रात है, जिसमें सभी भोग उसी प्रकार समा जाते हैं जिस प्रकार सभी जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले निर्विकार समुद्र में समा जाते हैं और जो परम शान्ति को प्राप्त कर ब्राह्मी-स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह स्थितप्रज्ञ ज्ञानी है (२/५५, ५७, ५९, ६९, ७० और ७२)। उसका आनन्द, उसकी शान्ति और उसका प्रकाश-ये सभी उसके अन्तरतम में निहित रहते हैं। वह सर्वभूतों में ईश्वर को और ईश्वर में सर्वभूतों को देखता है। उसकी समबुद्धि श्रेष्ठ तथा निकृष्ट में किसी भेद का दर्शन नहीं करती। उसे ईश्वर के दिव्य सान्निध्य का भान सर्वदा होता रहता है और वह उससे कभी विलग नहीं होता। उसके लिए कोई भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता; किन्तु वह अन्य लोगों के सम्मुख एक दृष्टान्त प्रस्तुत करने के लिए संसार के हितार्थ कर्म करता रहता है। संस्कृति के लक्ष्य का अनुमान उस स्थितप्रज्ञ पुरुष के भव्य दृष्टान्त से किया जा सकता है जिसके वैशिष्ट्य का वर्णन गीता के दूसरे, पाँचवें, छठे, बारहवें तथा चौदहवें अध्याय में किया गया है और जो स्वयं को उस प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करता है
जिसके अनुरूप प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति 'समन्ब्रह्म' में अपनी पूर्णता तथा कृतकृत्यता की सम्प्राप्ति की दिशा में अग्रसरण का अभीप्सु होता है।
गीता का सन्देश
गीता आशा, सान्त्वना, शान्ति तथा इन सबसे अधिक मनुष्य में अन्तर्भूत दिव्य तत्त्व का सन्देश है। यह प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है और उसे अभय प्रदान करती है। यह उसे दुःख-दारिद्रय के रसातल से ऊपर उठा कर अमरता तथा शाश्वत आनन्द के शिखर पर प्रतिष्ठित कर देती है। यह हमारे समक्ष जीवन के प्रति हिन्दू-दृष्टिकोण की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करती है। मानव-जीवन के बाह्य पक्ष पर रेखांकित उद्वेलनों के होते हुए भी भारत के अन्तरतम में समस्वरता और एकता का रुझान विद्यमान है। भारतीय शान्तिप्रिय तथा वैष्णव-जन होते हैं। भारतीय संस्कृति के ज्योति-स्तम्भ साधु-सन्त तथा अवतार ही भारत के महान् पुरुष हैं। मानव-चरित्र को सम्यक् दिशा प्रदान करने वाले भव्य धार्मिक आदर्शों, लोगों को सर्वोच्च पूर्णता के उत्तुंग शिखर पर अधिष्ठित करने वाले आचार-शास्त्र तथा नैतिकता के उदात्त सिद्धान्तों और मनुष्य को देवत्व के स्तर तक पहुँचाने वाले तथा राष्ट्रों के आध्यात्मिक जीवन का निर्देशन करने वाले आध्यात्मिक और उत्कृष्टतम सत्य का प्रादुर्भाव भारत में ही हुआ था। इतिहास में हमारा राष्ट्र भारत जब कभी भी आपत्तियों से आक्रान्त हुआ, तब भारतीय संस्कृति ने ही इसके अस्तित्व-रक्षण का उत्तरदायित्व वहन किया है। भगवद्गीता, जो उपनिषदों के उपदेशामृत का सारतत्त्व है, भारतीय जीवन का व्यावहारिक अनुदेश है और सर्वभूतों की संहति के लिए भारत यह प्रदेशन विश्व को प्रदान करता है। श्रीकृष्ण पूर्ण मानव के आदर्श, सगुण ईश्वर, साक्षात् सच्चिदानन्द, पूर्णावतार एवं संस्कृति, ज्ञान, शक्ति तथा आनन्द के शिरोबिन्दु हैं। वे गीता के माध्यम से विश्व को उच्चतम संस्कृति तथा आध्यात्मिक ज्ञान का सन्देश प्रदान करते हैं। यह भारत तथा विश्व के लिए गौरव की बात है कि गीता आत्माहुति, अनासक्ति और ईश्वर के प्रति आत्म-समर्पण की भावना से गृहस्थाश्रम में रह कर कर्म करते हुए लोगों को भी व्यक्ति तथा ईश्वर के तादात्म्य के उदात्त आदर्श से अनुप्राणित किया करती है।