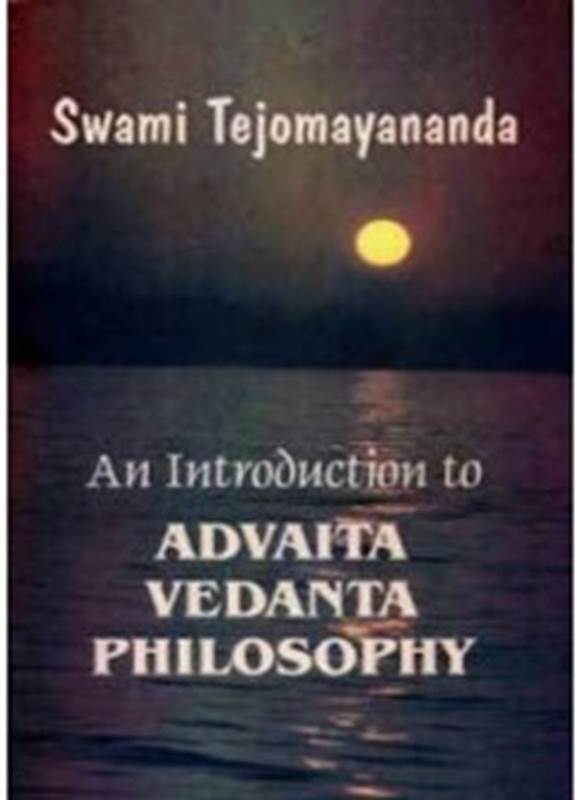
AN INTRODUCTION TO
ADVAITA VEDANTA
PHILOSOPHY
A Free Rendering into English of
‘Laghuvasudevamanana’
BY
SWAMI TEJOMAYANANDA
का हिन्दी अनुवाद
अद्वैत वेदांत दर्शन
एक परिचय
अनुवादक : रमेश चौहान
AN INTRODUCTION TO
ADVAITA VEDANTA
PHILOSOPHY
A Free Rendering into English of
‘Laghuvasudevamanana’
BY
SWAMI TEJOMAYANANDA

Published By
THE DIVINE LIFE SOCIETY,
P.O SHIVANANDANAGAR-249 192,
Distt. Tehri-Garhwal, U.P., Himalayas, India
1999
OM
Dedicated At The
Lotus Feet Of
Gurudev
Sri Swami Sivanandaji Maharaj
OM
विषय सूची
अनुबंध चतुष्टय और साधना चतुष्टय
बंधन की श्रृंखला I – पीड़ा और देहधारण
बंधन की श्रृंखला II – कर्म, प्रेम और घृणा
प्रेम और घृणा, आत्म-परिचय, अविवेक और अज्ञान
आत्मा तीनों शरीरों से भिन्न है
वर्णक 9 आत्मा तीनों अवस्थाओं का साक्षी है
परिशिष्ट I वेदांत बोध (श्री स्वामी शिवानंद)
'दशमस्त्वमसि'—'तू ही दसवाँ व्यक्ति है'
प्रकाशक का नोट
यह अपनी तरह का अनूठा प्रकाशन है, जिसे वेदान्त के उन विद्यार्थियों के लाभ के लिए जारी किया जा रहा है, जो अपने अध्ययन के प्रारंभिक चरण में हैं और जिन्हें ईश्वर, जगत और आत्मा की एकता के महान सिद्धांत के दर्शन का गैर-तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना है, जो धीरे-धीरे व्यवस्थित रूप से अनुभूति के स्तरों में प्रकट हो रहा है। इस मूल संस्कृत का पठनीय अंग्रेजी अनुवाद, जिसे 'लघुवासुदेवमनन' के नाम से जाना जाता है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, सिवाय एक के जो अब छपना बंद हो गया है। इस ग्रंथ के नए अनुवाद की आवश्यकता आश्रम के मुख्यालय में तब महसूस की गई, जब आश्रम के श्री स्वामी तेजोमयानंदजी महाराज ने इस पुस्तक के विषय पर अपने प्रवचन शुरू किए और विद्यार्थियों ने शिक्षण की रेखा का अनुसरण करने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस की। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, स्वामीजी ने शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त एक आसान शैली में, पाठ का संक्षिप्त अनुवाद करने का कष्ट उठाया है। हम वेदांत पर इस बहुमूल्य पुस्तिका को उन सभी लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जो भारत के प्राचीन ज्ञान के द्वार तक पहुँच प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं।
28.4.1999
-दि डिवाइन लाइफ सोसाइटी
भूमिका
आदि-गुरु भगवान नारायण, जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य तथा हमारे पूज्य सद्गुरु श्री स्वामी शिवानंदजी महाराज को नमन, जिनकी कृपा और आशीर्वाद परम श्रद्धेय स्वामी तेजोमयानंद सरस्वती पर बनी रहे, जिनके विद्वत्तापूर्ण अंग्रेजी प्रवचन, जो वेदांतिक ग्रंथ ‘लघुवासुदेवमनन’ पर आधारित हैं—जो कि वेदांत दर्शन का एक परिचयात्मक ग्रंथ है—इस पुस्तक की अत्यंत प्रकाशमान एवं शिक्षाप्रद विषयवस्तु का आधार हैं।
ये प्रवचन वेदांत के छात्रों के लिए उच्च स्तर के ग्रंथों का अध्ययन आरंभ करने के लिए एक उत्कृष्ट एवं अत्यंत उपयोगी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। स्वामी तेजोमयानंदजी की व्याख्याएँ और टिप्पणियाँ अपनी नवीन प्रस्तुति शैली, आधुनिक व्याख्यान पद्धति और सारगर्भित दृष्टांतों के माध्यम से जटिल विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत करने की विशेष विधि के कारण अद्वितीय हैं। इस पुस्तक को विशेष रूप से मूल्यवान बनाने में सम्मिलित चार्ट्स का भी विशेष योगदान है। इन सुंदर चित्रों को स्वामी तेजोमयानंदजी के निर्देशन में श्री स्वामी राजराजेश्वरानंदजी ने चित्रित किया है, जो इस अमूल्य योगदान के लिए हमारी बधाई के पात्र हैं।
साथ ही, इस प्रकाशन का संपूर्ण श्रेय स्वामी तेजोमयानंदजी की अत्यंत मेहनती और गंभीर छात्रा मैडम सिमोनेटा (पेरिस, फ्रांस) को जाता है, जिन्होंने मार्च 1971 में उनके कुछ प्रवचनों में भाग लिया था। मैडम सिमोनेटा ने उनके कक्षाओं के व्याख्यानों के विस्तृत नोट्स लिए और जब वे फ्रांस लौटीं, तो अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रति कृतज्ञता स्वरूप इस सामग्री को एक हस्तलिखित पांडुलिपि के रूप में संकलित किया। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस ग्रंथ को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का संकल्प लिया ताकि असंख्य वेदांत साधक एवं छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। इस ग्रंथ के पुस्तक रूप में प्रकाशन की संपूर्ण ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। उन्होंने स्वामीजी को अपनी पांडुलिपि पुनरावलोकन करने, संशोधित करने और इसे मुद्रण के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित किया।
मैडम सिमोनेटा ने वेदांत के इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने फ्रांसीसी सहधर्मियों के लिए सहज सुलभ बनाने के प्रयास में इसे फ्रेंच भाषा में भी अनुवादित कराया और यह पांडुलिपि भी मुद्रण के लिए तैयार है। उन्होंने एक योग्य शिक्षक की योग्य छात्रा होने का परिचय दिया है। उनके प्रयासों के कारण शुद्ध वेदांत का सच्चा ज्ञान पश्चिमी साधकों को उपलब्ध हो पाया है। वर्तमान समय में योग पश्चिम में एक फैशन और उन्माद बन चुका है, और अब यह आवश्यक हो गया है कि वहाँ शुद्ध वेदांत का प्रचार किया जाए। यह उनके जीवन में एक उचित दृष्टिकोण स्थापित करने में सहायक होगा और उनके जीवन में उच्च आध्यात्मिक गुणवत्ता को स्थान देगा। यह उनके बाह्य भौतिक एवं आंतरिक आध्यात्मिक जीवन के बीच उचित संतुलन स्थापित करने में सहायक होगा।
मैं इस ग्रंथ के व्यापक प्रचार-प्रसार और अधिकाधिक साधकों एवं जिज्ञासुओं द्वारा गंभीर अध्ययन की कामना करता हूँ। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। वेदांत का प्रकाश निरंतर प्रज्वलित रहे!
16-11-1972 स्वामी चिदानंद
भूमिका
‘अद्वैत वेदांत दर्शन का परिचय’ वह शीर्षक है जिसके अंतर्गत यहाँ वेदांत के तत्वमीमांसा पर विचार किया गया है। यह संस्कृत ग्रंथ ‘लघुवासुदेवमनन’ का सरल अंग्रेजी अनुवाद है, जो कि ‘वासुदेवमनन’ नामक व्यापक ग्रंथ का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ के लेखक का जीवन-परिचय इतिहास के अंधकार में विलुप्त हो गया है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत के अध्ययन के लिए एक सरल मार्गदर्शन एवं असीम प्रेरणा प्रदान करता है। इसे विद्वानों द्वारा अद्वैत वेदांत पर एक मानक संकलन माना जाता है।
इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद लंबे समय तक अंग्रेजी जानने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं था। जब मुझे ‘लघुवासुदेवमनन’ को पाठ्यपुस्तक के रूप में लेकर वेदांत के नवोदित छात्रों के लिए एक नियमित कक्षा संचालित करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मैंने इसकी आवश्यकता को गहराई से अनुभव किया, और परिणामस्वरूप यह प्रकाशन अस्तित्व में आया।
गुरुदेव स्वामी
शिवानंदजी महाराज कहते हैं:
"वेदांत अत्यंत व्यावहारिक विषय है। यह किसी स्वप्नद्रष्टा की कल्पना मात्र नहीं है। वेदांत का थोड़ा-सा भी ज्ञान,
नियमित और विधिपूर्वक किया गया अभ्यास तथा वेदांतिक भावना के अनुरूप जीने का एक विनम्र प्रयास भी महान भय को दूर कर सकता है, प्रचंड आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकता है और निर्विकार आनंद,
आत्मसुख, असीम पारलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान एवं अमरत्व की ओर अग्रसर कर सकता है...
वेदांत ब्रह्मविद्या है। यह मोक्ष-शास्त्र अथवा मुक्तिदर्शन है। वेदांत मनुष्य की मूल प्रकृति में उसकी महिमा को प्रकट करता है। संपूर्ण अस्तित्व की एकता का संदेश वेदांत देता है। वेदांत भारत की मूल संस्कृति है। यह भारत का राष्ट्रीय दर्शन है। यह भारतीय दर्शन का शिखर,
परमोत्कर्ष और चरम बिंदु है। इसने हिंदू समाज को पिछले आठ हजार वर्षों से जीवित रखा है..."
वेदों के अंतिम भाग अर्थात् उपनिषदों की विचारधारा को ‘वेदांत’ कहा जाता है। यह एक दर्शन है, क्योंकि यह सत्य की खोज करता है; किंतु यह केवल एक सैद्धांतिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष और अंतिम सत्य है, जो प्रमाणित एवं पुनः प्रमाणित किया जा सकता है। यह सभी ज्ञान-स्रोतों—श्रुति, युक्ति और अनुभव—का उपयोग करता है और जीवन के सभी अवस्थाओं एवं परिस्थितियों को अपने दायरे में समाहित करता है।
इस ग्रंथ में विचारधारा को निगमन (deduction) पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। परब्रह्म इसका प्रथम सिद्धांत (postulate) है, और सभी तत्व इसी से व्युत्पन्न होते हैं। सभी प्राच्य (पूर्वी) दार्शनिक इस बात से सहमत हैं कि परम तत्व (परब्रह्म) ही ज्ञात-अज्ञात समस्त वस्तुओं का एकमात्र सार है। इसलिए, ग्रंथ का प्रथम अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति अथवा विकास पर चर्चा करते हुए परब्रह्म को आधार मानकर प्रारंभ होता है, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांडों का अस्तित्व वर्तमान सृष्टि से पहले इसी एकमात्र वास्तविकता में विलीन हो गया था। ग्रंथ में एक उपमा दी गई है कि महाप्रलय के समय जीवात्माएँ परब्रह्म में उसी प्रकार स्थित रहती हैं, जैसे मोम के गोले में स्वर्ण-कण मिश्रित रहते हैं।
इस ग्रंथ में बारह वर्णकों (अध्यायों) में आत्मा (आत्मन्) के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की गई है और भ्रांतियों एवं मिथ्या पहचानों को दूर करने का प्रयास किया गया है। तीन शरीरों, तीन अवस्थाओं तथा पंचकोशों का वर्णन कर यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा इन सबसे भिन्न है। अंत में यह भी प्रमाणित किया गया है कि आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप तीन भिन्न गुणों का मिश्रण न होकर एक अविभाज्य, एकरस, स्वाभाविक सत्ता है।
छात्रों की शीघ्र और सरल समझ के लिए आवश्यकतानुसार चित्र, आरेख और सारणी सम्मिलित की गई हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान शंकराचार्यकृत ‘तत्त्वबोध’ का अंग्रेजी अनुवाद दिया गया है, जो वेदांत का एक संक्षिप्त विश्वकोश बनकर छात्रों को मुख्य ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। ग्रंथ के अंत में ‘वेदांत-बोध’ शीर्षक से स्वामी शिवानंदजी महाराज द्वारा संकलित कुछ प्रश्नोत्तर तथा एक शब्दावली (Glossary) भी पाठकों के लाभार्थ जोड़ी गई है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रंथ ज्ञान के जिज्ञासु साधकों के लिए वेदांत का एक उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध होगा और उन्हें इस विषय में गहराई से प्रवेश करने तथा परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।
मैं परम पूज्य स्वामी चिदानंदजी महाराज एवं स्वामी कृष्णानंदजी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय-समय पर मुझे प्रोत्साहित किया। इस प्रकाशन के लिए पाठकगण मैडम सिमोनेटा द’ सेसेरो (पेरिस, फ्रांस) के ऋणी हैं, जिनके उदार सहयोग से यह ग्रंथ प्रकाशित हो सका। मैं अपने गुरुभाइयों स्वामी ब्रह्मानंदजी, स्वामी राजराजेश्वरानंदजी (जिन्होंने पांडुलिपि संशोधित की और सुंदर आरेख बनाए) तथा श्री वेणुगोपालजी (जिन्होंने मुखपृष्ठ का उत्कृष्ट डिज़ाइन तैयार किया) का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।
शिवानंद आश्रम, स्वामी तेजोमयानंद
द डिवाइन लाइफ सोसाइटी मुख्यालय
22 जून, 1972
तत्त्वबोध
अपने गुरु वासुदेवेंद्र योगींद्र को नमन करते हुए, जो ज्ञान के प्रदाता हैं, मैं ‘तत्त्वबोध’ का उपदेश उन सभी मोक्ष-प्राप्ति के इच्छुक साधकों के कल्याण हेतु करता हूँ।
अब हम श्रेणियों के भेद की विधि का वर्णन करते हैं, जो साधन-चतुष्टय नामक चतुर्विध योग्यताओं से युक्त साधकों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है।
1. प्रश्न: साधन-चतुष्टय क्या है?
उत्तर: नित्य-अनित्य वस्तु-विवेक (शाश्वत एवं नश्वर वस्तुओं में भेदबुद्धि), वैराग्य (सांसारिक एवं पारलौकिक भोगों के प्रति उदासीनता), षट्सम्पत्ति (शम आदि छह गुण), तथा मुमुक्षुत्व (मोक्ष की तीव्र अभिलाषा) – ये चारों साधन-चतुष्टय कहलाते हैं।
2. प्रश्न: नित्य-अनित्य वस्तु-विवेक क्या है?
उत्तर: केवल एक अद्वितीय ब्रह्म ही नित्य है, तथा अन्य समस्त वस्तुएँ अनित्य हैं। इस प्रकार की भेदबुद्धि को नित्य-अनित्य वस्तु-विवेक कहते हैं।
3. प्रश्न: वैराग्य क्या है?
उत्तर: इस लोक और परलोक के भोगों की इच्छा का अभाव ही वैराग्य है।
4. प्रश्न: षट्सम्पत्ति क्या है?
उत्तर: ये छह प्रकार की
उत्कृष्ट योग्यताएँ हैं—
(a) शम, (b) दम,
(c) उपरति, (d) तितिक्षा,
(e) श्रद्धा, तथा (f) समाधान।
5. प्रश्न: शम क्या है?
उत्तर: मनोनिग्रह, अर्थात् मन का नियंत्रण शम कहलाता है।
6. प्रश्न: दम क्या है?
उत्तर: बाह्य इंद्रियों जैसे नेत्र, कान आदि का संयम दम कहलाता है।
7. प्रश्न: उपरति क्या है?
उत्तर: अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना उपरति कहलाता है।
8. प्रश्न: तितिक्षा क्या है?
उत्तर: शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति तितिक्षा कहलाती है।
9. प्रश्न: श्रद्धा क्या है?
उत्तर: गुरु एवं वैदिक ग्रंथों के वचनों में पूर्ण विश्वास को श्रद्धा कहते हैं।
10. प्रश्न: समाधान क्या है?
उत्तर: चित्त की एकाग्रता समाधान कहलाती है।
11. प्रश्न: मुमुक्षुत्व क्या है?
उत्तर: मोक्ष की तीव्र आकांक्षा को मुमुक्षुत्व कहते हैं।
12. प्रश्न: तत्त्व-विवेक क्या है?
उत्तर: आत्मा ही सत्य है, अन्य समस्त वस्तुएँ असत्य हैं—इस ज्ञान को तत्त्व-विवेक कहते हैं।
13. प्रश्न: आत्मा क्या है?
उत्तर: आत्मा वह है, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से भिन्न है, जो पंचकोशों से परे है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है और जिसका स्वरूप सत्-चित्-आनंद (शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद) है।
14. प्रश्न: स्थूल शरीर क्या है?
उत्तर: स्थूल शरीर पंच-महाभूतों के संयोग से
बना होता है। यह पूर्व
जन्मों के कर्मों का परिणाम
है। यह सुख-दुःख आदि अनुभव
करने का माध्यम है। यह
षड्विकारों (छह प्रकार के परिवर्तन)
से युक्त होता है—
(a) अस्ति (अस्तित्व),
(b) जायते (जन्म),
(c) वर्धते (वृद्धि),
(d) विपरिणमते (परिवर्तन),
(e) अपक्षीयते (क्षय), और
(f) विनश्यति (मृत्यु)।
15. प्रश्न: सूक्ष्म शरीर (सूक्ष्मशरीर) क्या है?
उत्तर: यह पाँच महाभूतों से बना है। यह सत्कर्म या भूतकाल के अच्छे कर्मों से उत्पन्न होता है। यह सुख, दुःख आदि का अनुभव करने का एक साधन है। इसमें पाँच ज्ञान-इंद्रियाँ या ज्ञान की इंद्रियाँ, पाँच कर्म-इंद्रियाँ या क्रिया के अंग, और पाँच प्राण या प्राण वायु के साथ-साथ मन और बुद्धि या बुद्धि, कुल मिलाकर सत्रह कलाएँ या श्रेणियाँ शामिल हैं। पाँच ज्ञान-इंद्रियाँ हैं: श्रोत्र या ध्वनि की इंद्री, त्वक या स्पर्श की इंद्री, चक्षु या दृष्टि की इंद्री, जिह्वा या स्वाद की इंद्री और घ्राण या गंध की इंद्री। स्रोत के अधिष्ठाता देवता दिग्देवता या दिशाओं के देवता हैं, त्वक के वायु या पवन-देवता हैं, चक्षु के सूर्य या सूर्य-देवता हैं, जिह्वा के वरुण या जल-देवता हैं, और घ्राण के दो अश्विनी-कुमार या देवों के जुड़वाँ चिकित्सक हैं। स्रोत का उद्देश्य शब्द या ध्वनि को ग्रहण करना है, त्वक का स्पर्श या स्पर्श है, चक्षु का रूप या रूप है, जिह्वा का रस या स्वाद है और घ्राण का गंध या गंध है। ज्ञान-इंद्रिय, अधिष्ठाता देवता और उनके संबंधित उद्देश्य नीचे सारणीबद्ध रूप में दिखाए गए हैं:
● पाँच ज्ञानेंद्रियाँ (इंद्रियाँ जो ज्ञान प्राप्त करती हैं),
● पाँच कर्मेंद्रियाँ (इंद्रियाँ जो कार्य करती हैं),
● पाँच प्राण (जीवन-शक्ति),
● मन (मनस) तथा
● बुद्धि।
पाँच ज्ञानेंद्रियाँ, उनके अधिष्ठाता देवता और उनके विषय इस प्रकार हैं:
|
ज्ञानेंद्रिय |
अधिष्ठाता देवता |
विषय |
|
श्रवण (कान) |
दिक्पाल (दिशाओं के देवता) |
शब्द (ध्वनि) |
|
त्वचा (स्पर्श) |
वायु देवता |
स्पर्श (संवेदन) |
|
चक्षु (नेत्र) |
सूर्य देवता |
रूप (रंग और आकार) |
|
जिह्वा (जीभ) |
वरुण देवता |
रस (स्वाद) |
|
घ्राण (नाक) |
अश्विनी कुमार (चिकित्सा देवता) |
गंध (सुगंध-दुर्गंध) |
पाँच कर्मेंद्रियाँ, उनके अधिष्ठाता देवता और उनके कार्य इस प्रकार हैं:
|
कर्मेंद्रिय |
अधिष्ठाता देवता |
कार्य |
|
वाक् (वाणी) |
अग्नि देवता |
बोलना |
|
पाणि (हाथ) |
इंद्र देवता |
वस्तुओं को ग्रहण करना |
|
पाद (पैर) |
विष्णु देवता |
गमन (चलना) |
|
पायु (गुदा) |
मृत्यु देवता |
मल त्याग |
|
उपस्थ (जननेंद्रिय) |
प्रजापति देवता |
भोग व प्रजनन |
16. प्रश्न: कारण शरीर क्या है?
उत्तर: कारण शरीर वह है, जो अवर्णनीय (निरूपण करने में असमर्थ), अनादि (जिसका कोई प्रारंभ नहीं) तथा अविद्या (अज्ञान) रूप है, जो अपरिवर्तनशील आत्मा को आच्छादित कर देता है तथा स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों का कारण बनता है।
17. प्रश्न: तीन अवस्थाएँ (अवस्था त्रय) क्या हैं?
उत्तर: तीन अवस्थाएँ इस प्रकार हैं—
(a) जाग्रत अवस्था (जागने की स्थिति),
(b) स्वप्न अवस्था (स्वप्न की स्थिति),
(c) सुषुप्ति अवस्था
(गहरी निद्रा की स्थिति)।
18. प्रश्न: जाग्रत अवस्था (जाग्रदवस्था) क्या है?
उत्तर: जाग्रत अवस्था वह स्थिति है, जिसमें इंद्रियों के माध्यम से बाहरी विषयों जैसे ध्वनि, रूप, गंध आदि को अनुभव किया जाता है। वह आत्मा जो इस अवस्था में स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है, उसे विश्व कहा जाता है।
19. प्रश्न: स्वप्न अवस्था (स्वप्नावस्था) क्या है?
उत्तर: जब सोने की अवस्था में चित्त में पूर्व में देखे एवं सुने हुए विषयों के संस्कारों के आधार पर अंतःकरण में एक सूक्ष्म, आभासी जगत उत्पन्न होता है, जिसमें द्रष्टा (देखने वाला) और दृश्य (देखी जाने वाली वस्तुएँ) दोनों ही व्यक्ति के भीतर उपस्थित होते हैं, उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। जो आत्मा इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करता है, उसे तैजस कहा जाता है।
20. प्रश्न: सुषुप्ति अवस्था (सुषुप्ति-अवस्था) क्या है?
उत्तर: वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है—"मैं कुछ नहीं जानता, मुझे गहरी और आनंदमय निद्रा प्राप्त हुई", उसे सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा कारण शरीर से तादात्म्य करता है और उसे प्राज्ञ कहा जाता है।
21. प्रश्न: पंचकोश (पाँच आवरण) क्या हैं?
उत्तर: ये पाँच प्रकार के
आवरण इस प्रकार हैं—
(a) अन्नमय कोश – अन्न
(भौतिक शरीर) का आवरण।
(b) प्राणमय कोश
– प्राणों (जीवन शक्ति)
का आवरण।
(c) मनोमय कोश – मन का आवरण।
(d) विज्ञानमय कोश
– बुद्धि का आवरण।
(e) आनंदमय कोश – आनंद
(कारण शरीर) का आवरण।
22. प्रश्न: अन्नमय कोश क्या है?
उत्तर: अन्नमय कोश वह है, जो अन्न के सार से उत्पन्न होता है, अन्न के द्वारा पोषित होता है, और मृत्यु के बाद पृथ्वी में विलीन हो जाता है।
23. प्रश्न: प्राणमय कोश क्या है?
उत्तर: पाँच प्राण (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान) तथा पाँच कर्मेंद्रियाँ मिलकर प्राणमय कोश का निर्माण करते हैं।
24. प्रश्न: मनोमय कोश क्या है?
उत्तर: मन तथा पाँच ज्ञानेंद्रियाँ मिलकर मनोमय कोश का निर्माण करती हैं।
25. प्रश्न: विज्ञानमय कोश क्या है?
उत्तर: बुद्धि तथा पाँच ज्ञानेंद्रियाँ मिलकर विज्ञानमय कोश का निर्माण करती हैं।
26. प्रश्न: आनंदमय कोश क्या है?
उत्तर: अविद्या (अज्ञान), जिसमें मलिन सत्त्व गुण रजस और तमस के मिश्रण के साथ उपस्थित रहता है, एवं जिसमें प्रिय, मोद, तथा प्रमोद नामक मानसिक वृत्तियाँ स्थित होती हैं, उसे आनंदमय कोश कहते हैं।
जैसे कंगन, झुमके और मकान आदि को हम "मेरा" कहकर आत्मा से भिन्न मानते हैं, उसी प्रकार पाँच कोश भी "मेरे" हैं, "मैं" नहीं। अतः आत्मा इन कोशों से अलग है।
27. प्रश्न: फिर आत्मा क्या है?
उत्तर: आत्मा सत्-चित्-आनंद स्वरूप है।
28. प्रश्न: सत् क्या है?
उत्तर: जो तीनों कालों (भूत, वर्तमान, भविष्य) में विद्यमान रहता है, उसे सत् (अस्तित्व) कहते हैं।
29. प्रश्न: चित् क्या है?
उत्तर: जो स्वयं प्रकाशित होकर समस्त जगत को प्रकाशित करता है, उसे चित् (चेतना) कहते हैं।
30. प्रश्न: आनंद क्या है?
उत्तर: जिसका स्वभाव ही आनंद है, उसे आनंद कहते हैं।
अतः, अपनी मूल प्रकृति को सत्-चित्-आनंद स्वरूप के रूप में जानो।
अब हम 24 तत्त्वों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाएंगे।
माया, जो ब्रह्म पर आश्रित है, तीन गुणों—सत्त्व, रजस और तमस—से बनी है। इससे क्रमशः उत्पन्न होते हैं—
● आकाश,
● वायु,
● अग्नि,
● जल,
● पृथ्वी।
इन पाँच तत्वों के सात्त्विक भाग से क्रमशः पाँच ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं—
● आकाश से – श्रवणेंद्रिय (कान),
● वायु से – स्पर्शेंद्रिय (त्वचा),
● अग्नि से – दृष्टि (नेत्र),
● जल से – रसना (जीभ),
● पृथ्वी से – घ्राण (नाक)।
इन्हीं तत्वों के सामूहिक सात्त्विक अंश से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की उत्पत्ति होती है।
राजसिक भाग से पाँच कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं—
● आकाश से – वाक् (वाणी),
● वायु से – पाणि (हाथ),
● अग्नि से – पाद (पैर),
● जल से – उपस्थ (जननेंद्रिय),
● पृथ्वी से – पायु (मलत्यागेंद्रिय)।
इन्हीं के सामूहिक राजसिक अंश से पाँच प्राण उत्पन्न होते हैं।
तामसिक भाग से पंचमहाभूतों का पंचीकरण (quintuplication) होता है।
31. प्रश्न: पंचीकरण (Panchikarana) क्या है?
उत्तर: प्रत्येक तामसिक तत्त्व को दो भागों में विभाजित किया जाता है—
● एक भाग ज्यों का त्यों रहता है।
● दूसरे भाग को चार भागों में विभक्त कर अन्य चार तत्वों में मिला दिया जाता है।
इस प्रक्रिया से पंचमहाभूतों का समिश्रण होता है, जिससे स्थूल शरीर की रचना होती है।
32.
प्रश्न: महावाक्य "तत्त्वमसि"
("That Thou Art") किस प्रकार
जीव, जो सीमित ज्ञान और
शरीर आदि के अहंकार से
युक्त है, तथा ईश्वर, जो सर्वज्ञ और शरीर आदि के
अहंकार से रहित है, के अद्वैत
(अभिन्नता) को स्थापित कर सकता है, जबकि उनके गुण एक-दूसरे के विपरीत
हैं?
उत्तर: "त्वम्" (तू) शब्द का वाच्यार्थ
(शाब्दिक अर्थ) जीव है, जो स्थूल और सूक्ष्म
शरीर का अभिमानी है, जो अविद्या (अज्ञान) और उसके प्रभावों से युक्त
है, तथा जो स्वयं को
शरीर और कर्ता के रूप
में मानता है। "त्वम्" शब्द का लक्ष्यार्थ
(संकेतार्थ) शुद्ध चैतन्य
(शुद्ध, निरपेक्ष चेतना)
है, जो अविद्या और उसके प्रभावों से
मुक्त है तथा समाधि अवस्था
में स्थित है।
इसी प्रकार, "तत्" (वह) शब्द का वाच्यार्थ ईश्वर है, जो माया और उसके प्रभावों से युक्त है तथा सर्वज्ञता (सर्वज्ञान) आदि गुणों से संपन्न है। "तत्" शब्द का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य है, जो माया और उसके प्रभावों से रहित है।
इस प्रकार, चूँकि एक अद्वितीय अखंड चैतन्य (अभिन्न चेतना) जीव और ईश्वर दोनों में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए जीव और ईश्वर के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं है।
33.
प्रश्न: जीवन्मुक्त कौन होते हैं?
उत्तर: वे जीवन्मुक्त कहलाते हैं जो वेदांत
वचनों (महावाक्यों) और गुरु के
उपदेशों के माध्यम से यह
प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं
कि—
"केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है,
और जीव स्वयं ब्रह्म है।"
जो व्यक्ति
यह दृढ़ निश्चयपूर्वक अनुभव कर लेता है
कि—
"मैं न तो ब्राह्मण हूँ,
न शूद्र हूँ, न पुरुष हूँ,
न स्त्री हूँ, बल्कि मैं तो अकर्ता (कर्तापन से रहित),
निर्विकल्प (निर्विकार), सत्-चित्-आनंद स्वरूप,
स्वप्रकाशित, सर्वव्यापक चेतना हूँ,"
वही जीवन्मुक्त कहलाता है।
यह प्रत्यक्ष ज्ञान कि "मैं ही वास्तव में ब्रह्म हूँ" (ब्रह्मैव अहमस्मि) सभी कर्मबंधन को समाप्त कर देता है।
34.
प्रश्न: कर्म कितने प्रकार के
होते हैं?
उत्तर: कर्म तीन प्रकार के
होते हैं—
(i) आगामी कर्म (वर्तमान में किए गए कर्म),
(ii) संचित कर्म (पिछले जन्मों के
संचित कर्म),
(iii) प्रारब्ध कर्म
(वर्तमान जन्म में भोगने योग्य
कर्म)।
35.
प्रश्न: आगामी कर्म क्या है?
उत्तर: ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी द्वारा
शरीर के माध्यम से किए
गए कर्म, जो पुण्य और
पाप के रूप में होते
हैं, आगामी कर्म कहलाते हैं।
36.
प्रश्न: संचित कर्म क्या है?
उत्तर: संचित कर्म वे समस्त
कर्म हैं, जो अनंत जन्मों
से संचित हैं और अभी
तक फलित नहीं हुए हैं।
वे सूक्ष्म संस्कारों के रूप में बीज
अवस्था में रहते हैं।
37.
प्रश्न: प्रारब्ध कर्म क्या है?
उत्तर: प्रारब्ध कर्म वे पुण्य
और पापमय कर्म हैं, जो पिछले जन्मों में
अर्जित किए गए थे और
जो इस वर्तमान शरीर के जन्म का
कारण बने हैं। इन प्रारब्ध कर्मों के
अनुसार ही सुख-दुःख के अनुभव
होते हैं।
यह प्रारब्ध कर्म केवल भोगने से ही समाप्त होता है।
संचित
कर्म ज्ञान की अग्नि द्वारा
नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी को यह
दृढ़ निश्चय होता है कि—
"मैं ब्रह्म हूँ, मैं इससे भिन्न कुछ नहीं हूँ।"
आगामी कर्म भी ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी का इन कर्मों से कोई संबंध नहीं होता, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की बूँद टिकती नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी इन कर्मों से अछूता रहता है।
इसके अतिरिक्त, जो लोग ज्ञानी की स्तुति, पूजन और सेवा करते हैं, वे उसके पुण्य कर्मों के भागी होते हैं, जबकि जो लोग उसे निंदा, द्वेष या कष्ट देते हैं, वे उसके पाप कर्मों के भागी बनते हैं।
इस प्रकार, आत्मज्ञानी (आत्मा के साक्षात् ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति) संसार रूपी समुद्र को पार कर ब्रह्मानंद (ब्रह्म का आनंद) को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है।
श्रुति (वेद) इस बात की
पुष्टि करते हुए कहती है—
"आत्मा को जानने वाला समस्त शोकों से मुक्त हो जाता है।" (तारति शोकम् आत्मवित्)
स्मृतियाँ भी कहती हैं कि ज्ञानी का शरीर चाहे काशी (बनारस) में त्यागा जाए या किसी चांडाल के घर में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वह पहले से ही मुक्त है और ज्ञान प्राप्ति के क्षण में ही सदा के लिए परम आनंद को प्राप्त कर लेता है।
अद्वैत वेदांत दर्शन
एक परिचय
वर्णक 1
उपोद्घात (प्रस्तावना)
प्रणाम वेदांत गुरु भगवन् श्री शंकराचार्य को, जो समस्त विद्याओं के आचार्य हैं, जो सत् (अस्तित्व) और आत्मा (स्व) की अद्वैतता को जानने वाले हैं।
मैं भगवान नारायण को नमन करता हूँ, जिन्होंने इस संसार में ऋषियों के हृदय को आनंदित करने के लिए आध्यात्मिक गुरु (वेदव्यास) के रूप में अवतार लिया, जो कृपा के सागर हैं, और जो अपने भक्तों के पापों को नष्ट करने वाले हैं।
अब मैं ‘मनन’ नामक ग्रंथ का संक्षिप्त प्रतिपादन करता हूँ, जिसे पूज्य ऋषि वासुदेव ने विस्तारपूर्वक व्याख्यायित किया है, अज्ञानियों के बोधार्थ एवं अपने आत्मिक ज्ञान को समृद्ध करने के उद्देश्य से।
भगवान श्रीकृष्ण, बाल-गोपाल, मेरे साथ रहें, मुझे इस कार्य में आशीर्वाद दें और सहायता करें।
जीवन के चार पुरुषार्थों—धर्म (सत्याचरण), अर्थ (धन-संग्रह), काम (इच्छाओं की पूर्ति) और मोक्ष (जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति) में, केवल मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि वही नित्य है। "वह फिर लौटकर नहीं आता, वह फिर लौटकर नहीं आता" (छां.उ. VIII-xv-1) ऐसा श्रुति कहती है। अन्य तीन नित्य नहीं हैं, क्योंकि वे अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। "जिस प्रकार इस संसार में कर्मों द्वारा प्राप्त किया गया लोक नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार परलोक में भी पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त किया गया लोक नष्ट हो जाता है" (छां.उ. VIII-i-6), ऐसा श्रुति कहती है।
मोक्ष केवल आत्मा के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। "उस परम तत्व को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है; मोक्ष का और कोई उपाय नहीं है" (श्वे.उ. VI-15)। "ब्रह्म को जानने वाला परम पद को प्राप्त करता है" (तैत्त.उ. II-1), ऐसा श्रुति कहती है।
इस ब्रह्म या परम सत्य का साक्षात्कार ‘अध्यारोप’ (आरोपण) और ‘अपवाद’ (निरोध) की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। क्योंकि आधारभूत तत्व का ज्ञान तभी संभव है जब आरोपित तत्व को निष्प्रभावी किया जाए। "सत्य का निर्णय अध्यारोप और अपवाद के द्वारा किया जाना चाहिए।" "ज्ञानी लोग अमृतत्व को न तो कर्मों से, न संतान से और न ही धन से प्राप्त करते हैं, बल्कि संन्यास के द्वारा प्राप्त करते हैं," ऐसा कैवल्योपनिषद (2) कहती है। इसलिए सत्य के साधकों को इस अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया को अवश्य समझना चाहिए।
संदेह: ‘अध्यारोप’ का क्या अर्थ है?
स्पष्टीकरण: जिस प्रकार शुक्ति में चाँदी का भ्रम होता है, रस्सी में साँप का आभास होता है, स्तंभ में मनुष्य का आभास होता है, उसी प्रकार ब्रह्म या आत्मा में इस समस्त ब्रह्मांड की मिथ्या प्रतीति होती है। इसे ‘अध्यारोप’ कहते हैं। यह भ्रांति वास्तविकता के अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। यह अज्ञान ही विभिन्न रूपों में जाना जाता है, जैसे अविद्या (मूल अज्ञान), तमस (अंधकार), मोह (मायाजाल), मूलप्रकृति (सृष्टि का आदिकारण), प्रधान (प्रकृति का मूल तत्व), गुण-साम्य (त्रिगुणों की सम अवस्था), अव्यक्त (अव्यक्त शक्ति), और माया (मिथ्या प्रत्यक्ष शक्ति)।
मूलप्रकृति तीन गुणों—सत्त्व, रजस और तमस—का संयोजन है, जिसे सफेद, लाल और काले रंग की तीन रस्सियों से बनी हुई एक रस्सी के रूप में कल्पना की जा सकती है। इसे ‘प्रलय’ (सृष्टि का संहार) और ‘महा-सुषुप्ति’ (कारण निद्रा) भी कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, असंख्य जीवात्माएँ अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के सूक्ष्म संस्कारों सहित मूलप्रकृति में सुप्त अवस्था में रहती हैं, जैसे मोम के गोले में स्वर्ण-कण समाए रहते हैं।
यह अनुभव सभी जीवों को गहरी निद्रा में प्राप्त होता है…
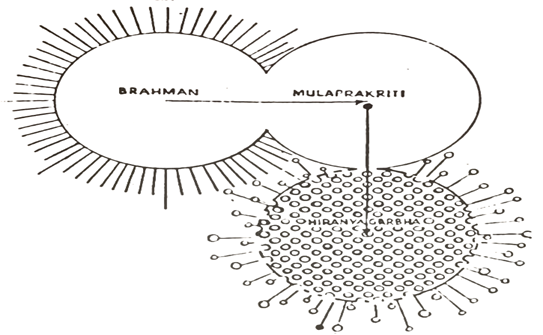
चित्र 1 ब्रह्मांडीय परिवार
ब्रह्मांडीय परिवार
प्रकृति मेरी देखरेख में चर और अचर सृष्टि को उत्पन्न करती है; इस कारण, हे अर्जुन, यह संसार चक्र निरंतर घूमता रहता है… जानो कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, और यह भी जानो कि सभी विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। — गीता (IX-10, XIII-19)
"मेरा गर्भ महत् ब्रह्म है; उसमें मैं बीज का संचार करता हूँ; वहाँ से, हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का जन्म होता है। जो भी रूप किसी भी गर्भ में उत्पन्न होते हैं, उनका गर्भस्थल महत् ब्रह्म ही है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ।" — गीता (XIV-3 & 4)
सुषुप्ति अवस्था (गहरी नींद की अवस्था)
सृष्टि के प्रारंभ में मूलप्रकृति स्वयं को तीन भागों में विभाजित करती है, जिन्हें माया, अविद्या और तामसी कहा जाता है। यह विभाजन जीवों के पूर्व कर्मों के संस्कारों के कारण होता है, जो अभिव्यक्ति के लिए तैयार होते हैं। इसमें माया में सतोगुण अन्य दो गुणों (रजस और तमस) की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है।
साक्षात् चेतना, जो सृष्टि से पूर्व भी 'अस्तित्व' में होती है, जब माया में प्रतिबिंबित होती है, तब उसे 'ईश्वर' या 'सामूहिक कारण स्वरूप' कहा जाता है। इसे 'अव्यक्त' (अविभाजित) और 'अंतर्यामिन्' (अंतर में निवास करने वाला) भी कहा जाता है। यही सम्पूर्ण ब्रह्मांड का सृजनकर्ता है। यह पूर्ण चेतना-सत्ता है। यही चेतना-सत्ता जब तमस द्वारा सीमित होती है, तब यह ब्रह्मांड की 'उपादान कारण' या भौतिक कारण बन जाती है। इसे स्वयं में और सृष्टि के संबंध में देखने पर यह उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि एक मकड़ी अपने जाले के लिए न केवल सूत्र उत्पन्न करती है बल्कि उसे बुनती भी है।
ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को कैसे रचा? इसे इस प्रकार समझाया गया है: पूर्व उल्लिखित अविद्या में रजोगुण प्रमुख होता है और यह असंख्य रूपों में प्रकट होती है तथा यह अनंत होती है। इसलिए 'साक्षात् चेतना' के प्रतिबिंब के रूप में जीव भी अनंत संख्या में होते हैं। व्यक्तिगत अज्ञान या 'व्यष्टिरूप अविद्या' और सामूहिक मूलप्रकृति या 'समष्टिरूप मूलप्रकृति' क्रमशः जीवों और ईश्वर के कारण शरीर (कारण शरीर) बनते हैं।
जीवों और ईश्वर के कारण शरीर का स्थान सुषुप्ति अवस्था (गहरी नींद की अवस्था) है। उनका कारण शरीर आनंदमय कोश या ब्लिस-शीथ बन जाता है। इस प्रकार कारण जगत की रचना होती है।
सूक्ष्म जगत की सृष्टि:
ईश्वर की इच्छा से मूलप्रकृति के तमोगुण ने दो भागों में विभाजन किया - 'आवरण शक्ति' (ढंकने की शक्ति) और 'विक्षेप शक्ति' (प्रक्षेपण शक्ति)। केवल विक्षेप शक्ति से सूक्ष्म आकाश (सुक्ष्म आकाश) उत्पन्न हुआ। सूक्ष्म आकाश से सूक्ष्म वायु (सुक्ष्म वायु) उत्पन्न हुई। सूक्ष्म वायु से सूक्ष्म अग्नि (सुक्ष्म अग्नि) उत्पन्न हुई। सूक्ष्म अग्नि से सूक्ष्म जल (सुक्ष्म आपस) उत्पन्न हुआ। सूक्ष्म जल से सूक्ष्म पृथ्वी (सुक्ष्म पृथ्वी) उत्पन्न हुई।
इन पाँच तत्त्वों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे सूक्ष्म तत्त्व (सुक्ष्म भूत), अपंचीकृत तत्त्व (अपंचीकृत भूत), तथा तन्मात्राएँ (तन्मात्राएँ)। अज्ञान या कारण अज्ञान (मूलप्रकृति) से तीन गुण प्रकट हुए: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
सूक्ष्म शरीर (लिंग देह) की उत्पत्ति इस प्रकार होती है:
व्यष्टि या व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक सूक्ष्म तत्त्व के सतोगुण भाग से पाँच ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न हुईं: शब्द तन्मात्रा से श्रवण (सुनने की शक्ति), स्पर्श तन्मात्रा से स्पर्श (स्पर्श करने की शक्ति), रूप तन्मात्रा से दृष्टि (देखने की शक्ति), रस तन्मात्रा से स्वाद (स्वाद ग्रहण करने की शक्ति) और गंध तन्मात्रा से गंध (सूंघने की शक्ति)।
समष्टि या सामूहिक स्तर पर सूक्ष्म तत्त्वों के सतोगुण भाग से 'अंतःकरण' उत्पन्न हुआ। यह चार भागों में विभाजित होता है: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इनमें अहंकार को बुद्धि के अंतर्गत और चित्त को मन के अंतर्गत रखा जाता है।
इसी प्रकार, सूक्ष्म तत्त्वों के रजोगुण के व्यष्टि स्तर से पाँच कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुईं: वाणी (बोलने की शक्ति), हस्त (ग्रहण करने की शक्ति), पाद (गमन करने की शक्ति), उपस्थ (संतान उत्पत्ति करने की शक्ति) और गुदा (त्याग करने की शक्ति)। इनके समष्टि स्तर से प्राण या जीवन शक्ति उत्पन्न हुई, जो पाँच भागों में विभाजित होती है: प्राण (श्वास), अपान (त्याग), व्यान (परिसंचरण), उदान (उर्ध्वगति) और समान (संतुलन बनाए रखने की शक्ति)।
ये सत्रह तत्त्व मिलकर सूक्ष्म शरीर या लिंग देह का निर्माण करते हैं। यही भोग का उपकरण है। सूक्ष्म शरीर में जीव की अवस्था 'स्वप्न अवस्था' कहलाती है। इसमें तीन कोश विद्यमान होते हैं - विज्ञानमय कोश (बुद्धि कोश), मनोमय कोश (मनस कोश) और प्राणमय कोश (प्राण कोश)। इस प्रकार सूक्ष्म जगत की सृष्टि होती है।
स्थूल जगत की सृष्टि:
पाँच अपंचीकृत सूक्ष्म तत्त्वों में से प्रत्येक स्वयं को दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग स्वयं के लिए रखता है और दूसरे भाग को चार बराबर भागों में बाँटकर प्रत्येक अन्य तत्त्व में वितरित करता है। यह प्रक्रिया 'पंचीकरण' कहलाती है। इस प्रकार पाँच तन्मात्राएँ पंचीकृत होकर स्थूल महाभूत (स्थूल तत्त्व) बनती हैं।
इन्हीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसमें चौदह लोक होते हैं: भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। चार प्रकार के स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं - अंडज (अंडे से जन्मे), जरायुज (गर्भ से जन्मे), स्वेदज (पसीने से उत्पन्न) और उद्भिज (बीज से उत्पन्न)। इसके अतिरिक्त सभी भौतिक भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जीव और ईश्वर के भौतिक शरीरों का स्थान जाग्रत अवस्था (जागने की स्थिति) है। यह स्थूल अभिव्यक्ति अन्नमय कोश (भौतिक शरीर) के रूप में प्रकट होती है।
इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि संपन्न होती है।
हर एक शरीर - कारण, सूक्ष्म और स्थूल - दो प्रकार के होते हैं: व्यष्टि (व्यक्तिगत) और समष्टि (सामूहिक)। ईश्वर समष्टि उपाधि का धारक है, जबकि जीव व्यष्टि उपाधि का धारक है।
ईश्वर तीन गुणों - रजस, सतोगुण और तमस - के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता है।
माया और अविद्या के प्रभाव से अज्ञान उत्पन्न होता है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म को आच्छादित कर देता है। इस अज्ञान का नाश ही मोक्ष की प्राप्ति का कारण बनता है। वेदांत का अंतिम निष्कर्ष यह है कि 'ब्रह्म ही सत्य है और मैं वही हूँ' - इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला मुक्त कहलाता है।
सारांश
तीन गुणों
का उद्भव और उनसे उत्पन्न
तत्त्व:
मूलप्रकृति से
उत्पन्न अज्ञान से तीन गुण
- सत्त्व, रजस और तमस प्रकट
हुए। इन गुणों के व्यष्टि
रूप में:
● सत्त्व गुण के पाँच सूक्ष्म तत्वों से पाँच ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न हुईं –
○ शब्द तन्मात्रा से श्रवणेंद्रिय (कान),
○ स्पर्श तन्मात्रा से स्पर्शेंद्रिय (त्वचा),
○ रूप तन्मात्रा से दृष्टि (नेत्र),
○ रस तन्मात्रा से जिह्वा (स्वाद),
○ गंध तन्मात्रा से घ्राणेंद्रिय (नाक)।
समष्टि रूप में सत्त्व गुण से अंतःकरण (अंतर्मन) उत्पन्न हुआ, जो चार भागों में विभाजित है -
1. मन (संकल्प-विकल्प करने वाला),
2. बुद्धि (निर्णय करने वाली शक्ति),
3. अहंकार (स्वयं की अनुभूति),
4.
चित्त (स्मृति)।
अहंकार को बुद्धि का भाग
और चित्त को मन का
भाग माना जाता है।
कर्मेंद्रियाँ और
प्राणों की उत्पत्ति:
रजोगुण के व्यष्टि रूप से पाँच कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुईं
–
1. वाणी (बोलने की शक्ति),
2. पाणि (हाथ - ग्रहण करने की शक्ति),
3. पाद (पैर - चलने की शक्ति),
4. उपस्थ (जननेंद्रिय),
5. गुदा (त्याग करने की शक्ति)।
समष्टि रूप से रजोगुण से प्राण उत्पन्न हुआ, जो पाँच प्रकार का है –
1. प्राण (श्वसन क्रिया),
2. अपान (त्याग क्रिया),
3. व्याण (शरीर में ऊर्जा का संचार),
4. उदान (ऊर्ध्वगमन करने वाला प्राण),
5. समान (पाचन क्रिया में सहायक)।
स्थूल ब्रह्मांड
(स्थूल सृष्टि) की उत्पत्ति:
पाँच अपंचीकृत सूक्ष्म तत्व, जो तमस प्रधान
होते हैं, दो भागों में
विभाजित होते हैं
–
● एक भाग स्वयं को बनाए रखता है।
●
दूसरा भाग चार बराबर भागों
में विभाजित होकर अन्य चार
तत्वों में मिल जाता है।
इस मिश्रण को पंचीकरण (Quintuplication) कहा
जाता है। इन पंचीकृत तत्वों
से स्थूल भूत उत्पन्न होते
हैं, जिससे स्थूल ब्रह्मांड (ब्रह्माण्ड) का निर्माण होता
है।
तीन प्रकार के शरीर (कारण, सूक्ष्म, स्थूल) का समष्टि और व्यष्टि रूप:
● समष्टि = संपूर्ण शरीरों का योग।
● व्यष्टि = एकल शरीर।
● समष्टि कारण शरीर = ईश्वर (ईश्वर),
● व्यष्टि कारण शरीर = प्राज्ञ (व्यष्टि जीव),
● समष्टि सूक्ष्म शरीर = हिरण्यगर्भ,
● व्यष्टि सूक्ष्म शरीर = तैजस,
● समष्टि स्थूल शरीर = वैश्वानर या विराट पुरुष,
● व्यष्टि स्थूल शरीर = विश्व।
त्रिगुणात्मक सृष्टि
चक्र:
ईश्वर तीन गुणों के आधार
पर सृष्टि, पालन और संहार
करते हैं –
● रजोगुण से – ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता),
● सत्त्वगुण से – विष्णु (पालक),
● तमोगुण से – रुद्र (संहारक)।
अज्ञान का
नाश और मोक्ष की प्राप्ति:
अज्ञान (अविद्या) से संसार का
भ्रम उत्पन्न होता है।
इस भ्रम को नष्ट करने
के लिए दो प्रकार के
ज्ञान आवश्यक हैं
–
1. परोक्ष ज्ञान (श्रवण, मनन) – जिससे सत्य का अस्तित्व बोध होता है।
2. अपरोक्ष ज्ञान (निदिध्यासन, साक्षात्कार) – जिससे स्वयं को ब्रह्म जानने का प्रत्यक्ष अनुभव होता है।
इस प्रकार, मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया सात अवस्थाओं में पूर्ण होती है –
1. अज्ञान,
2. आवरण शक्ति,
3. विक्षेप शक्ति,
4. परोक्ष ज्ञान,
5. अपरोक्ष ज्ञान,
6. दुखों का अंत,
7. परम आनंद की प्राप्ति।
वर्णक 2
अनुबंध चतुष्टय और साधना चतुष्टय
इस दूसरे अध्याय में एक उत्तम ग्रंथ के चार अनिवार्य तत्वों का वर्णन किया गया है, जिन्हें अनुबन्ध चतुष्टय कहा जाता है। ये हैं (i) विषय या प्रतिपाद्य तत्व, (ii) प्रयोजन या लाभ, (iii) सम्बन्ध या ग्रंथ तथा प्रतिपाद्य विषय के बीच का नाता, और (iv) अधिकारी या योग्य विद्यार्थी। वेदांत साहित्य में विषय ब्रह्म या परम सत्य है, और मोक्ष या मुक्ति इसका प्रयोजन है। सम्बन्ध का तात्पर्य प्रतिपाद्य और प्रतिपादन के बीच की कड़ी से है, अर्थात् ब्रह्म और वेदांत ग्रंथ, जो इसे स्पष्ट करता है। जो साधन चतुष्टय से सम्पन्न है, वही योग्य विद्यार्थी है।
जिस प्रकार केवल ब्राह्मण ही बृहस्पतिसवन यज्ञ करने के अधिकारी होते हैं और केवल क्षत्रिय ही राजसूय यज्ञ कर सकते हैं, उसी प्रकार वही व्यक्ति वेदांत का अध्ययन कर सकता है, जो साधन चतुष्टय से सम्पन्न हो। ये चार गुण हैं (i) विवेक, अर्थात् नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच का भेदभाव, (ii) वैराग्य, अर्थात् इस लोक और परलोक में कर्मों के फलभोग के प्रति विरक्ति, (iii) षट्सम्पत्तियाँ, जैसे शम (मानसिक नियंत्रण) आदि, और (iv) मुमुक्षुत्व, अर्थात् जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने की तीव्र इच्छा।
विवेक का अर्थ यह ज्ञान है कि ब्रह्म ही नित्य है और यह संसार अनित्य है। यह ज्ञान श्रुति (वेद), स्मृति (धर्मशास्त्र), पुराण आदि के अध्ययन से सहज रूप से प्राप्त होता है। वैराग्य का अर्थ इंद्रियजनित सुखों जैसे पुष्प, चंदन आदि के प्रति तथा स्वर्गीय अप्सराओं और अन्य लौकिक सुखों के प्रति अरुचि रखना है, क्योंकि ये सभी क्षणिक और त्याज्य हैं, जैसे कुत्ते की उल्टी, मूत्र और मल। षट्सम्पत्तियाँ छह गुणों से युक्त होती हैं, जो इस प्रकार हैं: (i) शम, (ii) दम, (iii) उपरति, (iv) तितिक्षा, (v) समाधान और (vi) श्रद्धा।
शम का तात्पर्य मन को श्रवण (आध्यात्मिक विषयों को सुनना या अध्ययन करना) की ओर स्थिर करना और इसे अन्य सांसारिक विषयों से दूर रखना है। दम का अर्थ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का संयम करना है। उपरति का तात्पर्य सभी सांसारिक गतिविधियों से निवृत्ति है, जिसमें त्याग और निष्काम सेवा भी शामिल हैं। तितिक्षा का अर्थ सुख-दुःख, गर्मी-सर्दी आदि द्वंद्वों को सहन करना है, जो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। समाधान का तात्पर्य मन को सदा आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन में स्थिर रखना है। श्रद्धा का अर्थ गुरु और वेदांत के प्रति अटूट विश्वास रखना है। मुमुक्षुत्व का अर्थ सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की प्रबल इच्छा रखना है, जिसमें ऐषणात्रय (काम, धन और संतान की इच्छा) का त्याग किया जाता है। यह वैसा ही होता है जैसे जलते हुए घर में फंसा व्यक्ति किसी भी तरह बाहर निकलने की तीव्र इच्छा रखता है, भले ही उसे अपनी पत्नी, बच्चे या अन्य लोगों को छोड़ना पड़े।
इस संसार में यह देखा जाता है कि विवेक होने पर भी कुछ व्यक्तियों में वैराग्य की कमी होती है, इसलिए यह आवश्यक बताया गया है कि इस लोक और परलोक के कर्मफल से विरक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार, कुछ संत प्रकृति के लोगों में भी क्रोध, पीड़ा आदि देखी जाती है, यद्यपि वे विवेक और वैराग्य से युक्त होते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि षट्सम्पत्तियों को भी धारण किया जाए। कुछ व्यक्तियों में विवेक, वैराग्य और षट्सम्पत्तियाँ होते हुए भी वे ज्ञान मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं होते और वे सगुण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए, मुमुक्षुत्व का होना भी आवश्यक बताया गया है।
जो विद्यार्थी उपर्युक्त गुणों से युक्त होता है, उसे समिधा (यज्ञीय ईंधन) और गुरु के लिए दक्षिणा लेकर अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और श्रद्धा व सम्मानपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। फिर उसे गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए: 'हे प्रभु! हे महापुरुष! हे अज्ञान नाशक! जीव कौन है? ईश्वर कौन है? यह विश्व क्या है? ये तीनों किससे उत्पन्न होते हैं? और इस संसार बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है?' यह शास्त्रों का भी आदेश है: 'जो ब्राह्मण (अर्थात् आध्यात्मिक साधक) कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त लोकों की परीक्षा करके उनमें वैराग्य प्राप्त कर ले, उसे समझना चाहिए कि अकृतक (स्वयंभू ब्रह्म) कर्मों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए समिधा लेकर उस गुरु के पास जाना चाहिए, जो वेदों में पारंगत हो और ब्रह्म में स्थित हो' (मुण्डक उपनिषद् 1.2.12)। 'प्रणाम, सेवा और बार-बार प्रश्न करने से तत्वदर्शी ऋषि तुम्हें उस ज्ञान की शिक्षा देंगे' (भगवद्गीता 4.34)। जब शिष्य इस प्रकार विनम्रतापूर्वक प्रश्न करता है, तब गुरु कृपापूर्वक उसे जीव, ईश्वर और विश्व के बीच के अंतर को समझाते हैं, जो कि सत्व, रजस और तमस नामक तीन गुणों के द्वारा भिन्न-भिन्न होता है। इसके पश्चात् गुरु उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, उतनी ही स्पष्टता से जितना कोई हाथ की हथेली में रखे आँवले के फल को देख सकता है।
यह समझना चाहिए कि उपर्युक्त चार साधन भगवान की कृपा और असंख्य जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यह भी जान लेना चाहिए कि जो गुरु ब्रह्मज्ञान प्रदान करता है, वह वास्तव में स्वयं परमेश्वर ही होता है।
जो व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन से आत्मा और परमात्मा के अभेद को समझता है, वही मुक्ति प्राप्त करता है। यही सिद्धांत अटल और निश्चित है।
सारांश
अनुबंध चतुष्टय
(i) विषय
(ग्रंथ में वर्णित विषय-वस्तु),
(ii) प्रयोजन (ग्रंथ के अध्ययन से
प्राप्त होने वाला लाभ),
(iii) संबंध (ग्रंथ और विषय-वस्तु के बीच संबंध),
और
(iv) अधिकारी (जो इस ग्रंथ को
पढ़ने के योग्य है)।
वेदांत साहित्य में विषय ब्रह्म (परम सत्य) है, प्रयोजन मोक्ष (जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति) है, संबंध व्याख्येय (ब्रह्म) और उसकी व्याख्या (ग्रंथ) के बीच का संबंध है, तथा अधिकारी वह साधक है, जो साधना चतुष्टय के चार गुणों से संपन्न है।
साधना चतुष्टय
(i) विवेक
(नित्य और अनित्य वस्तुओं में
भेद करने की क्षमता),
(ii) वैराग्य (इस लोक और परलोक
के कर्मफल से उत्पन्न सुखों
के प्रति उदासीनता),
(iii) षट्सम्पत्ति (छः आंतरिक गुण—शम, दम,
उपरति, तितिक्षा, समाधान,
श्रद्धा), तथा
(iv) मुमुक्षुत्व (मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा)।
षट्सम्पत्ति
(i) शम
– मन को सांसारिक विषयों से हटाकर श्रवण
(वेदांत अध्ययन) में स्थिर रखना।
(ii) दम – ज्ञानेंद्रियों
और कर्मेंद्रियों
को वश में रखना।
(iii) उपरति – सभी सांसारिक कर्तव्यों से निवृत्ति। इसमें
त्याग और निष्काम सेवा भी सम्मिलित हैं।
(iv) तितिक्षा – प्रारब्ध कर्म के कारण
उत्पन्न सुख-दुःख,
शीत-उष्ण आदि द्वंद्वों को
सहन करने की क्षमता।
(v) समाधान – मन को हमेशा आत्मज्ञान प्राप्ति की
ओर केंद्रित रखना।
(vi) श्रद्धा – गुरु और वेदांत शास्त्रों के वचनों
में अटूट विश्वास।
वर्णक 3
आत्मा और अनात्मा
संदेह: यह विश्व कितने तत्वों
से बना है?
स्पष्टीकरण: यह विश्व दो तत्वों
से बना है—आत्मा
(स्व) और अनात्मा
(अस्व)।
संदेह: आत्मा, जो कि इस
विश्व से परे है, फिर भी इसमें कैसे
समाविष्ट होती है?
स्पष्टीकरण: चूँकि यह ब्रह्मांड चेतन
और जड़ दोनों प्रकार की
सत्ताओं से बना है, और चेतनता आत्मा का
स्वभाव है, इसलिए आत्मा का
ब्रह्मांड में समावेश अपरिहार्य है।
यदि ऐसा न हो, तो यह ब्रह्मांड ही
अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसलिए,
ब्रह्मांड में आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार
करना आवश्यक है।
संदेह: चेतन (संवेदनशील) और जड़
(असंवेदनशील) तत्व कौन-कौन से हैं?
स्पष्टीकरण: समस्त गतिशील वस्तुएँ चेतन
हैं, और सभी अचल वस्तुएँ
जड़ हैं।
संदेह:
जब ये दोनों—चेतन और जड़—इतने अधिक और
विविध हैं, तो ब्रह्मांड केवल
दो भागों में कैसे बाँटा
जा सकता है?
स्पष्टीकरण: अनात्मा (अस्व)
वास्तव में एक ही है;
यह केवल अपने विभिन्न प्रभावों के कारण
अनेक प्रतीत होता है। इसी
प्रकार, आत्मा (स्व)
भी एक ही है, किंतु यह जीवों और
ईश्वरों के रूप में विभिन्न
उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत
होती है, जो कि अनात्मा
के प्रभावस्वरूप निर्मित होती हैं।
संदेह: एक ही ईश्वर अनेक
रूपों में कैसे प्रकट होता
है?
स्पष्टीकरण: ईश्वर के अनेक रूपों
का यह विचार केवल विभिन्न
मूर्तियों और प्रतिमाओं के माध्यम से उत्पन्न
होता है, जैसे कि शिव,
विष्णु आदि की छवियाँ, जो तीर्थस्थानों, गाँवों, घरों आदि में पूजी
जाती हैं।
संदेह:
क्या मिट्टी, पत्थर आदि से
बनी मूर्तियों में ईश्वरत्व की
कल्पना की जा सकती है?
स्पष्टीकरण: हाँ, यदि इन मूर्तियों में ईश्वरत्व निहित न
होता, तो लोग इतनी कठिनाई
उठाकर, इतना धन खर्च करके
उनका अभिषेक, नैवेद्य आदि क्यों करते? यहाँ यह कहना अप्रासंगिक होगा कि
गैर-हिंदू इन मूर्तियों की
पूजा नहीं करते। इस विषय
में केवल आस्थावान लोगों के दृष्टांत को
ही उदाहरण के रूप में
लिया जाना चाहिए। आखिर, जब लोग इस भौतिक
शरीर को ही आत्मा मानने
का भ्रम पाल सकते हैं,
जबकि यह मल-मूत्र से भरा
हुआ है, तो फिर इन
पवित्र और ऊर्जामय मूर्तियों में ईश्वरत्व देखने
में क्या आपत्ति हो सकती
है?
संदेह:
क्या कोई ऐसा उदाहरण है,
जिससे यह सिद्ध हो सके
कि अनात्मा अपने प्रभावों के
कारण अनेक रूपों में प्रकट
होती है, और आत्मा भी
अनात्मा के प्रभाव से निर्मित
उपाधियों के माध्यम से अनेक
प्रतीत होती है?
स्पष्टीकरण: हाँ, जैसे पृथ्वी अपने
विभिन्न रूपांतरणों के माध्यम से
अलग-अलग रूपों में प्रकट
होती है—जैसे पर्वत, वृक्ष, स्तंभ,
दीवार, अनाज का भंडार, घर, मठ,
मिट्टी के बर्तन आदि—वैसे ही मूलप्रकृति, जो स्वयं अनात्मा है,
अनेक रूपों में प्रकट होती
है।
जैसे आकाश, जो अविभाज्य है, पृथ्वी के विभिन्न रूपांतरणों जैसे—घड़ा, घर आदि—में प्रवेश कर घटाकाश (घड़े में स्थित आकाश), गृहाकाश (घर में स्थित आकाश) आदि नामों से जाना जाता है, वैसे ही अद्वितीय आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा, जो कि मूलप्रकृति के प्रभावस्वरूप निर्मित होते हैं, उनमें प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। अज्ञानी लोग इसे विभिन्न रूपों में देखते हैं—जैसे कि राम, कृष्ण आदि दिव्य स्वरूप, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, पक्षी, कीट, कीड़े आदि सांसारिक स्वरूप। इस प्रकार, आत्मा अनेक प्रतीत होती है।
यह दृष्टिकोण आवच्छिन्न पक्ष (उपाधियों द्वारा सीमित चेतना का सिद्धांत) के आधार पर दिया गया है।
अब प्रतिबिंब पक्ष (यह सिद्धांत कि जीवात्मा परमात्मा का अंतःकरण में प्रतिबिंब मात्र है) के आधार पर निम्नलिखित दृष्टांत दिए जा सकते हैं—
जैसे एक ही जल अनेक रूपों में प्रतीत होता है—जैसे महासागर, नदी, तालाब, कुएँ का जल, घड़े का जल आदि—वैसे ही एक ही अनात्मा (मूलभूत शक्ति) विभिन्न रूपों में प्रकट होती है।
जैसे एक ही सूर्य महासागर, तालाब आदि में अनेक प्रतिबिंबों के रूप में दिखाई देता है, वैसे ही एक ही आत्मा अनेक शरीरों के अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर अनेक प्रतीत होती है।
संदेह: आत्मा और जीवात्मा के
इस संबंध को कैसे समझा
जा सकता है?
स्पष्टीकरण: जैसे घटाकाश
(घड़े का आकाश)
और महाकाश (सर्वव्यापी आकाश) में कोई भेद
नहीं है, वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा में भी
कोई भेद नहीं है।
संदेह: यदि जीवात्मा केवल कल्पित या प्रतिबिंबित सत्ता है,
तो वास्तविक परमात्मा और अवास्तविक जीवात्मा को एक कैसे
कहा जा सकता है? क्या यह सत्य और
असत्य को समान मानने जैसा
नहीं होगा?
स्पष्टीकरण: जीवात्मा के तीन स्तर
होते हैं—
(i) परमार्थिक स्तर
(अद्वितीय सत्य),
(ii) व्यवहारिक स्तर
(सापेक्षिक यथार्थ), और
(iii) प्रतीतिमान स्तर
(मिथ्या स्वरूप)।
ये तीनों स्तर तीन अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं...
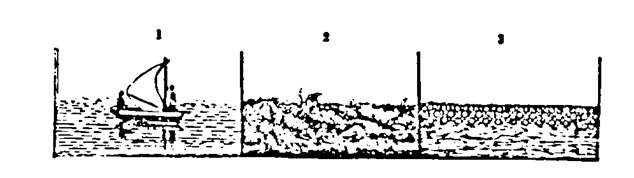
चित्र 2. जीव के तीन पहलू
जीव के तीन रूप
1. परमार्थिक जीव (गहरी निद्रा की अवस्था) – जैसे शांत जल।
2. व्यवहारिक जीव (जाग्रत अवस्था) – जैसे जल में उत्पन्न तरंगें।
3. प्रतीभासिक जीव (स्वप्न अवस्था) – जैसे तरंगों से उत्पन्न झाग।
ये तीनों अवस्थाएँ क्रमशः (i) गहरी निद्रा, (ii) जाग्रत, और (iii) स्वप्न के अनुरूप हैं।
जिस प्रकार जल में अस्थायी रूप से तरंगें उत्पन्न होती हैं और तरंगों से झाग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार व्यवहारिक जीव (व्यक्तिगत चेतना) परमार्थिक जीव (शुद्ध चेतना) से प्रकट होता है, और प्रतीभासिक जीव (मिथ्या चेतना) व्यवहारिक जीव से प्रकट होता है।
जिस प्रकार जल की तरलता, शीतलता और स्वाद, जो जल के स्वाभाविक गुण हैं, तरंगों में प्रकट होते हैं और फिर तरंगों के माध्यम से झाग में भी प्रकट होते हैं, उसी प्रकार परमार्थिक जीव (जिसका आधार शुद्ध ब्रह्म है) के सत् (अस्तित्व), चित् (चेतना) और आनंद (परमानंद) के गुण व्यवहारिक जीव में प्रकट होते हैं और फिर व्यवहारिक जीव के माध्यम से प्रतीभासिक जीव में भी प्रकट होते हैं।
जिस प्रकार बिना तरंगों के झाग का अस्तित्व नहीं होता, और बिना जल के तरंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार बिना व्यवहारिक जीव के प्रतीभासिक जीव का कोई अस्तित्व नहीं होता, और बिना परमार्थिक जीव के व्यवहारिक जीव का कोई अस्तित्व नहीं होता। केवल परमार्थिक जीव ही वास्तविक और शाश्वत है।
इसलिए, जैसे घटाकाश (घड़े के भीतर का आकाश) वास्तव में महाकाश (सर्वव्यापक आकाश) से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार जीवात्मा का परमार्थिक स्वरूप वास्तव में परमात्मा से भिन्न नहीं है। यही वेदांत का अंतिम निष्कर्ष है।
इस प्रकार, जो साधक 'नेति-नेति' (न यह, न यह) के सिद्धांत द्वारा पंचकोशों—अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक—से परे स्थित परमार्थिक सत्ता को अलग करके उसे अपने 'स्व' के रूप में पहचानता है, और श्रुति (वेदों) के गहन अध्ययन और तर्कसंगत विवेक द्वारा यह प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ही अद्वितीय ब्रह्म हूँ), वही व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।
समस्त उपनिषदें एक स्वर में घोषणा करती हैं कि ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति पुण्य और पाप—दोनों से मुक्त हो जाता है।
वर्णक 4
बंधन की श्रृंखला I – पीड़ा और देहधारण
व्यक्तिगत आत्मा
(जीव) जन्म-मरण के चक्र
में एक श्रृंखला द्वारा बंधी हुई है,
जिसके सात प्रमुख कड़ियाँ हैं—
(i) पीड़ा (दुःख)
(ii) देहधारण (शरीर प्राप्ति)
(iii) कर्म (क्रिया)
(iv) राग-द्वेष (प्रेम और घृणा)
(v) स्वरूप की
भ्रांति (अहंता-अभिमान)
(vi) विवेकाभाव (अविवेक)
(vii) अज्ञान (अविद्या)
इन्हें 'बंधन की श्रृंखला' कहा जाता है। इस श्रृंखला में प्रत्येक उत्तरवर्ती कड़ी अपने से पहले वाली कड़ी का कारण होती है। इस अध्याय और अगले अध्याय में प्रारंभिक चार कड़ियों का विश्लेषण किया जाएगा।
संदेह: क्या पीड़ा (दुःख) हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है, या यह बाह्य (अतिरिक्त) है?
स्पष्टीकरण: यह केवल बाह्य तत्व है। यदि इसे आत्मा का स्वाभाविक गुण मान लिया जाए, तो इससे कई असंगत निष्कर्ष उत्पन्न होंगे।
संदेह: वह कैसे?
स्पष्टीकरण: यदि पीड़ा जीवात्मा का स्वाभाविक स्वभाव होती, तो—
1. कभी भी दुःख का नाश नहीं हो सकता था।
2. किसी भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती थी।
3. कोई भी व्यक्ति अपने दुःखों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता।
4. कोई भी पुण्यकर्म करने, योग-साधना करने, ध्यान, उपासना आदि करने का प्रयास नहीं करता।
5. वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती।
संदेह: क्या यह संभव नहीं है कि दुःख मनुष्यों के लिए स्वाभाविक हो और वे उससे मुक्ति पाने का प्रयास करें?
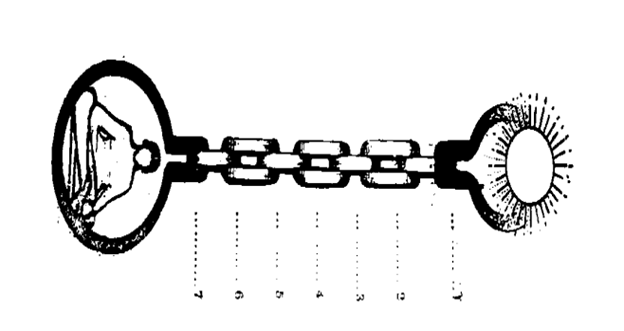
चित्र 3: बंधन की श्रृंखला
बंधन की श्रृंखला
1. अज्ञान (Ajnana) – अज्ञानता
2. अविवेक (Aviveka) – विवेक का अभाव
3. अभिमान (Abhimana) – अहंकार और आसक्ति
4. राग-द्वेष (Raga-Dvesha) – प्रेम और घृणा
5. कर्म (Karma) – कर्म और उसके फल
6. जन्म (Janma) – देहधारण
7. दुःख (Duhkha) – पीड़ा और कष्ट
स्पष्टीकरण: नहीं, यह संभव नहीं है कि दुःख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण हो। यदि यह उसका मूल स्वभाव होता, तो कोई भी व्यक्ति इसे समाप्त करने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि कोई भी अपनी वास्तविकता को मिटाने का प्रयास नहीं करता। यदि किसी की स्वाभाविक सत्ता ही समाप्त हो जाए, तो वह अपने जीवन के इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकता है?
संदेह: कोई व्यक्ति अपने स्वभाव (स्वरूप) को अपनी वास्तविकता क्यों मानेगा?
स्पष्टीकरण: इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। मिठास चीनी का स्वाभाविक गुण है। यदि मिठास को उससे अलग कर दिया जाए, तो चीनी स्वयं नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार, यदि पीड़ा जीवात्मा का स्वाभाविक गुण होती, तो पीड़ा के विनाश के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती।
परंतु आत्मा नाश रहित और शाश्वत है। शास्त्रों में कहा गया है—
● "आत्मा अविनाशी है।" (बृहदारण्यक उपनिषद् IV-v-14)
● "वह आकाश की भांति सर्वव्यापी और शाश्वत है।"
● "न तो वह जन्म लेती है और न मरती है। वह कहीं से उत्पन्न नहीं होती और न ही किसी वस्तु में बदलती है। वह अजन्मा, नित्य, अविनाशी और प्राचीन है, तथा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती।" (कठोपनिषद् I-ii-18)
इसलिए यह सिद्ध होता है कि पीड़ा आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं, बल्कि बाह्य (अतिरिक्त) है।
संदेह: क्या किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण समाप्त होने के बाद भी उसका वास्तविक स्वरूप बना रह सकता है?
स्पष्टीकरण: नहीं, ऐसा संभव नहीं है।
संदेह: जिस प्रकार किसी जादुई पत्थर या मंत्रों के प्रभाव से अग्नि की ऊष्मा समाप्त हो सकती है, बिना अग्नि को नष्ट किए, और वह स्पर्श में ठंडी भी हो सकती है, उसी प्रकार, यदि पीड़ा जीवात्मा का स्वाभाविक गुण होती, तो उसे योग, उपासना, तथा उच्च कर्मों के माध्यम से नष्ट किया जा सकता था, और आत्मा एक नए गुण—सुख—को प्राप्त कर सकती थी।
स्पष्टीकरण: यदि ऐसा होता, तो आत्मा को प्राप्त होने वाला सुख स्थायी नहीं रहता, बल्कि अस्थायी होता।
संदेह: यह क्यों?
स्पष्टीकरण: जो कुछ भी कर्मों द्वारा उत्पन्न होता है, वह कर्मों के समाप्त होते ही लुप्त हो जाता है।
उपरोक्त उदाहरण में—
● अग्नि और आत्मा अपनी ऊष्मा और पीड़ा को अस्थायी रूप से जादुई पत्थर या पुण्य कर्मों के कारण खो सकते हैं।
● परंतु जब उन उपायों और कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वही स्वाभाविक गुण (गर्मी और पीड़ा) पुनः प्रकट हो जाएंगे।
इसलिए, यदि हम यह मान लें कि पीड़ा जीव का स्वाभाविक गुण है, तो इसका अर्थ यह होगा कि मोक्ष केवल क्षणिक होगा, स्थायी नहीं।
यह शास्त्रों के उन वचनों के विरुद्ध होगा, जो कहते हैं—
● "जो मोक्ष प्राप्त करता है, वह कभी लौटकर नहीं आता।"
● "आत्मा अखंड, आनंदमय, निराकार और अद्भुत है।"
इसके अलावा, यदि पीड़ा जीवात्मा का स्वाभाविक गुण होती, तो वह गहरी निद्रा, समाधि और शांति की अवस्था में भी बनी रहती। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता।
जब
कोई व्यक्ति गहरी निद्रा, समाधि, या मानसिक शांति
से जागृत होता है, तो वह अनुभव करता
है—
"मैं अब तक सुखी था।"
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि—
1. सुख ही आत्मा का स्वाभाविक गुण है।
2. दुःख केवल एक बाह्य प्रभाव है।
3. जब जीव देह धारण करता है, तभी वह पीड़ा का अनुभव करता है।
क्योंकि "जहाँ देहधारण है, वहाँ पीड़ा है।" यही प्रकृति का नियम है।
संदेह:
क्या राजा, राजकुमार आदि भी केवल देहधारण
के कारण पीड़ा का अनुभव
करते हैं?
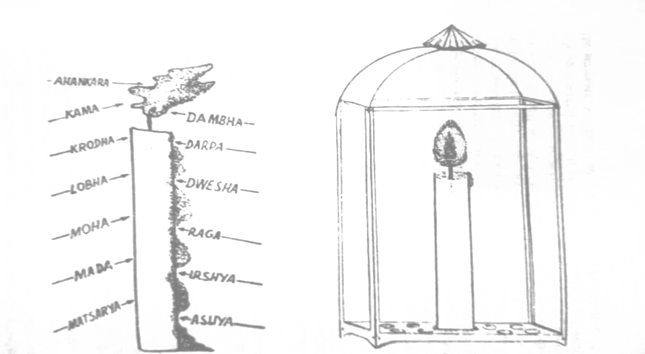
चित्र 4:अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर
अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर
स्पष्टीकरण: हाँ, राजा, राजकुमार और अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति भी देहधारण के कारण दुःख का अनुभव करते हैं। उनके दुःख विभिन्न रूपों में होते हैं, जैसे—
● शत्रुओं द्वारा उत्पीड़न,
● राज्य की ज़िम्मेदारियों का बोझ,
● धन और संपत्ति की हानि,
● प्रियजनों की मृत्यु,
● वृद्धावस्था, और
● अपनी स्वयं की मृत्यु।
यह केवल एक भ्रम है कि कुछ लोग इस संसार में पूर्ण रूप से सुखी हैं।
संदेह: भ्रम किस प्रकार दुःख को सुख में बदल सकता है?
स्पष्टीकरण: जैसे एक कुली, जो अपने सिर पर भारी बोझ लेकर तेज़ी से दौड़ता है, एक किसान या अन्य श्रमिक अपने कठिन परिश्रम को आनंद मान लेते हैं और अपने कार्य को हँसते-गाते हुए करते हैं। यही भ्रम है, जिसके कारण वास्तविक रूप से पीड़ा देने वाली परिस्थितियाँ भी सुखद प्रतीत होती हैं।
संदेह: क्या विवेकी (बुद्धिमान) व्यक्ति भी देहधारण के कारण पीड़ा का अनुभव करते हैं?
स्पष्टीकरण: हाँ, वे भी भूख, प्यास, गर्मी, ठंड, बीमारियाँ, बिच्छू और साँप के डंक, शेर आदि के आक्रमण के कारण शारीरिक पीड़ा का अनुभव करते हैं।
संदेह: तब फिर अज्ञानी और विवेकी व्यक्ति में क्या अंतर है?
स्पष्टीकरण: बाह्य रूप से देखने पर इनमें अधिक अंतर नहीं दिखाई देता, किंतु आंतरिक समझ और अनुभव के स्तर पर इनके बीच अत्यधिक भिन्नता होती है। विवेकवान एवं ज्ञानयुक्त व्यक्ति शास्त्रों की वाणी, तर्क और अनुभव द्वारा सहायता प्राप्त कर इस संसार में रहते हैं। वे इस प्रकार तर्क करते हैं— "संपूर्ण पीड़ा अंतःकरण की है, न कि आत्मा की। आत्मा का स्वरूप सत्-चित्-आनंद (शुद्ध अस्तित्व-चेतना-परमानंद) है, जबकि अंतःकरण का स्वरूप असत्यता, जड़ता और पीड़ा है।" शास्त्रों में कहा गया है— "असंगो ह्ययं पुरुषः" अर्थात् "यह आत्मा किसी भी वस्तु से असंबद्ध है" (बृहदारण्यक उपनिषद IV-iii-15)। तर्क द्वारा हम उसे अवयव-रहित, सत्य और शाश्वत के रूप में पहचानते हैं। गहरी निद्रा, शांत अवस्था और समाधि के अनुभव द्वारा भी हम इसे सत्य मानते हैं।
किन्तु, अविवेकी और अज्ञानी व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप की जांच किए बिना शरीर आदि को ही आत्मा मान लेता है। वह स्वयं के वास्तविक गुणों का स्थानांतरण अहंकार और देह में कर देता है और स्वयं को जाति, रंग, संप्रदाय आदि के आधार पर पहचानता है। इस प्रकार, वह सोचता है— "मैं देवता हूँ", "मैं मनुष्य हूँ", "मैं आंध्र निवासी हूँ", "मैं तमिल हूँ", "मैं ब्राह्मण हूँ", "मैं क्षत्रिय हूँ", "मैं वैश्य हूँ", "मैं शूद्र हूँ", "मैं ब्रह्मचारी हूँ", "मैं गृहस्थ हूँ", "मैं वानप्रस्थी हूँ", "मैं संन्यासी हूँ" आदि। इस प्रकार विवेकी और अविवेकी के बीच महान अंतर होता है। जब हम इस विषय की और गहराई से जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि बाह्य कर्मों के स्तर पर भी इन दोनों में समानता नहीं होती।
संदेह: यह कैसे?
स्पष्टीकरण: विवेकशील मनुष्य, व्यक्त जगत की मिथ्याता को जानकर, स्वप्न में भोगने के समान अपने 'प्रारब्ध' भोग को भी मिथ्या मानता है; जबकि अज्ञानी मनुष्य जगत के साथ-साथ जीव के दुःख-सुख को भी वास्तविक मानता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि देह-सुख में भी निश्चित रूप से दुःख है, यहाँ तक कि विवेकशील व्यक्तियों के मामले में भी। देह-सुख के कारण देवों या देवों को भी दुःख होता है, जिसका संकेत 'वज्रहस्त: पुरंदर:' जैसे शास्त्रों में मिलता है - 'देवताओं के स्वामी इन्द्र अपने हाथ में वज्र धारण करते हैं।'
● विवेकी व्यक्ति इस जगत को मिथ्या मानते हैं और अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख-दुःख का अनुभव वैसे ही करते हैं जैसे स्वप्न में किए गए अनुभव को देखते हैं।
● अज्ञानी व्यक्ति इस संसार और उसमें प्राप्त सुख-दुःख को सत्य मानते हैं और इनसे स्वयं को बाँध लेते हैं।
इसलिए सिद्ध होता है कि देहधारण में पीड़ा तो होती ही है, यहाँ तक कि विवेकी व्यक्ति के लिए भी।
संदेह: क्या देवता भी पीड़ा का अनुभव करते हैं?
स्पष्टीकरण: हाँ, देवता भी देहधारण के कारण पीड़ा का अनुभव करते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है:
● "वज्रहस्तः पुरंदरः" – "स्वर्ग के राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करते हैं।"
● यह संकेत करता है कि वे भी झगड़ों, क्रोध, शाप, और दैत्यों के आक्रमण से पीड़ित होते हैं।
● वे अपने पुण्य कर्मों के समाप्त होने के बाद पुनः जन्म लेने के भय से भी बँधे रहते हैं।
संदेह: यदि देवता भी पीड़ा के अधीन हैं, तो वे पूजनीय और मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाले कैसे हो सकते हैं?
स्पष्टीकरण: उदाहरण के लिए, राजाओं और समृद्ध लोगों को ही लें। यद्यपि वे स्वयं अपनी पीड़ाओं के अधीन होते हैं, फिर भी वे अपने प्रजा जनों और आश्रितों की पीड़ा को दूर करने और उन्हें आनंद प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं जैसे कि "स्वर्गलोक में देवता आनंदमय होते हैं", जो विपरीत अर्थ का संकेत देते प्रतीत होते हैं। लेकिन इन वचनों का वास्तविक तात्पर्य यह है— "अंतःकरण के गुणों के रूप में पीड़ा को जानकर, वे स्वर्गलोक में अपने आनंदमय स्वरूप का अनुभव करते हैं।"
इसके अलावा, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि "ये देवता भी सृष्ट होकर इस विशाल संसार-सागर में गिर पड़े" (ऐतरेय उपनिषद II-1), जो स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि देवताओं के लिए भी शरीर धारण करने के साथ-साथ पीड़ा का संयोग अनिवार्य है। इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति को शरीर के बंधनों से मुक्त होकर विदेहमुक्ति या पूर्ण मोक्ष की अवस्था प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।
संदेह: यदि मोक्ष का अर्थ
हमेशा देह से मुक्त होना
है, तो वे कुछ दिव्य
आत्माएँ जो हमें आकाश में
तारों के रूप में दिखाई
देती हैं, उन्हें मुक्त आत्माएँ
क्यों कहा जाता है?
स्पष्टीकरण: मोक्ष के चार प्रकार होते हैं— (i) सालोक्य, अर्थात जिस देवता की उपासना की जाती है, उसी लोक में निवास करना, (ii) सामीप्य, अर्थात उस देवता के समीप रहना, (iii) सारूप्य, अर्थात उस देवता के समान स्वरूप धारण करना, और (iv) सायुज्य, अर्थात उस देवता में पूर्णतः लय हो जाना। इन चारों प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग मार्ग बताए गए हैं— सालोक्य मोक्ष चैर्या (ईश्वर की सेवा और समर्पण) से, सामीप्य मोक्ष क्रिया (शिव, विष्णु आदि देवताओं की उपासना) से, सारूप्य मोक्ष योग (यम, नियम आदि अष्टांग योग के अभ्यास) से, और सायुज्य मोक्ष ज्ञान (जीवात्मा और परमात्मा की एकता का साक्षात्कार) से प्राप्त होता है। पहले तीन प्रकार की मुक्तियों का बहुत अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि इन स्थितियों में पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। केवल अंतिम प्रकार की मुक्ति ही सर्वोत्तम और वांछनीय मानी जाती है, क्योंकि इसमें पुनर्जन्म नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है, "योगेन सायुज्यम्" अर्थात 'योग के माध्यम से परमात्मा से एकत्व'। शरीर रहित मोक्ष को मात्र शून्यता या अस्तित्वहीनता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति देह रहते हुए मुक्त होता है, वह दूसरों को दिखाई देता है, जबकि देह के नष्ट होने के बाद मुक्त हुए व्यक्ति को कोई देख नहीं सकता, फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। जिस प्रकार गहरी निद्रा में आनंद अनुभव किया जाता है लेकिन उसका कोई रूप नहीं होता, उसी प्रकार मोक्ष के आनंद का अनुभव केवल आत्मा स्वयं कर सकती है, परंतु वह दूसरों के लिए दृश्य नहीं होता।
संदेह:
यदि मोक्ष का आनंद और
गहरी निद्रा का आनंद एक
समान है, तो क्या हम
गहरी निद्रा को मोक्ष मान
सकते हैं?
स्पष्टीकरण: ऐसा कदापि नहीं है।
इसे इस रूप में नहीं
समझना चाहिए। यद्यपि अद्वैत आनंद
के अनुभव की दृष्टि से
गहरी निद्रा और मोक्ष की
स्थिति में समानता प्रतीत हो
सकती है, फिर भी गहरी
निद्रा में अज्ञान बना रहता
है और व्यक्ति बाद में जाग्रत अवस्था
में लौट आता है, जबकि मोक्ष में न
तो अज्ञान रहता है और
न ही कोई पुनरावृत्ति होती
है। अतः मोक्ष की प्राप्ति मात्र गहरी
निद्रा से नहीं हो सकती।
इसी प्रकार, महाप्रलय (जब समस्त जीव अव्यक्त अवस्था में अपने संचित संस्कारों के साथ सुप्त रहते हैं) को भी मोक्ष की स्थिति नहीं समझना चाहिए। यह भी गहरी निद्रा के समान ही है, जिसमें अज्ञान बना रहता है और अगले कल्प (सृष्टि चक्र) में जीव फिर से प्रकट होते हैं। परंतु मोक्ष का आनंद व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है, यह मात्र एक शून्यता नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है।
संदेह: यदि देह रहते हुए मुक्त पुरुष (जीवन्मुक्त) और शरीर त्याग कर मुक्त हुए पुरुष (विदेहमुक्त) दोनों ही आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है?
स्पष्टीकरण: मुख्य अंतर यह है कि विदेहमुक्त अवस्था में अज्ञान और उसके प्रभावों का पूर्णतः नाश हो जाता है तथा कोई पुनरागमन नहीं होता। जबकि जीवन्मुक्त अवस्था में व्यक्ति को शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट सहने पड़ते हैं, यद्यपि वह उन्हें स्वप्नवत समझता है और उनसे प्रभावित नहीं होता।
हमने श्रुति (शास्त्रों) और युक्ति (तार्किक विश्लेषण) के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि विदेहमुक्ति ही परम आनंद की अवस्था है, जबकि शरीर के बने रहने से विभिन्न प्रकार की पीड़ाएँ बनी रहती हैं। अब हम अनुभव (अनुभूति) के आधार पर भी इसे प्रमाणित करेंगे।
गहरी निद्रा में प्रत्येक व्यक्ति को शरीर-बोध के अभाव के कारण किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। दूसरी ओर, जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं में सभी को शरीर-बोध के कारण कष्टों का अनुभव होता है। इसलिए, यह सार्वभौमिक सत्य है कि जहाँ कहीं शरीर होगा, वहाँ कष्ट भी होंगे। आत्मा, जो स्वभावतः आनंदस्वरूप है, भी शरीर धारण करने पर कष्ट का अनुभव करती है, यद्यपि यह कष्ट आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है।
संदेह: इस शरीरधारण का कारण क्या है?
स्पष्टीकरण: शरीरधारण का कारण केवल पंचभूत (पाँच महाभूतों) का संयोग नहीं है, क्योंकि ये पंचभूत संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, फिर भी जहाँ-जहाँ वे पाए जाते हैं, वहाँ शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। बल्कि जब पंचभूत जीव के संचित कर्मों के साथ संयोग करते हैं, तब शरीर का निर्माण होता है।
संदेह: क्या यह नहीं कहा जा सकता कि शरीर का निर्माण पुरुष के शुक्र (वीर्य) और स्त्री के शोणित (डिंब) के संयोग से होता है, जो कि पंचभूतों के विकार ही हैं?
स्पष्टीकरण: ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कई बार शुक्र और शोणित के संयोग के बावजूद भी शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए, शरीर का वास्तविक कारण केवल पंचभूत नहीं, बल्कि वे पंचभूत जो संचित कर्मों से जुड़े होते हैं, वे ही शरीर निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं।
अब, चूँकि पंचभूत, आकाश और समय सार्वभौमिक रूप से विद्यमान हैं, अतः विभिन्न प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति केवल जीवों के कर्मों की विभिन्नताओं के कारण ही संभव होती है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, जबकि मिट्टी तो सर्वत्र एक ही होती है, उसी प्रकार पंचभूत भी सर्वत्र एक समान होते हुए भी, जब वे जीवों के भूतकालीन कर्मों के साथ संयोग करते हैं, तभी विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। अन्यथा, सभी शरीर एक ही प्रकार के होने चाहिए—एक ही जाति, रंग, आकार, विशेषताएँ, ऊँचाई, जीवनकाल आदि में समान।
जिस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में मिट्टी उपादान कारण (सामग्री) है और कुम्हार निमित्त कारण (कर्म करने वाला) है, उसी प्रकार यहाँ पंचभूत उपादान कारण हैं और जीवों के संचित कर्म निमित्त कारण हैं। जब तक संचित कर्म फल देने के लिए तैयार रहते हैं, तब तक शरीर प्राप्त होता रहता है। इसी कारण स्वप्न और जाग्रत अवस्थाओं में शरीर का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर आवश्यक होता है। जब कर्मों की समाप्ति हो जाती है, तब शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसा कि गहरी निद्रा में होता है।
इसी प्रकार, जब तक मिट्टी उपलब्ध होती है, तब तक केवल मिट्टी के होने मात्र से बर्तन नहीं बनते, जब तक कि कुम्हार का प्रयत्न न हो। इसी प्रकार, जब तक ईश्वर द्वारा उत्पन्न किए गए पंचभूत विद्यमान हैं, तब तक यदि किसी जीव के कर्म समाप्त हो जाएँ, तो उसे फिर कभी शरीर प्राप्त नहीं होगा और वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा।
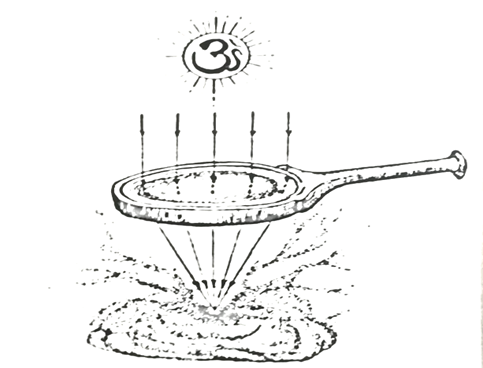
चित्र 5 : अंतःकरण रूपी लेंस के माध्यम से ज्ञान की अग्नि, अज्ञान के कपास को भस्म कर देती है
संदेह: विभिन्न शास्त्रों में भूतकाल के कर्मों के प्रभाव के बारे में अलग-अलग कथन क्यों हैं? कुछ कर्मकांड संबंधी शास्त्रों में कहा गया है कि "चाहे पुण्य हो या पाप, किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे करोड़ों कल्प (सृष्टि चक्र) बीत जाएँ, भोगे बिना किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता।" वहीं ज्ञान से संबंधित शास्त्रों में कहा गया है कि "ज्ञान की अग्नि सभी पूर्व कर्मों को उनके फलों सहित भस्म कर देती है" (गीता IV-7)। इन विरोधाभासी शास्त्र वचनों में से किसका अनुसरण करना चाहिए?
स्पष्टीकरण: शास्त्रों में दो प्रकार के वचन होते हैं— (i) प्रबल वचन (बलशाली या निर्णायक कथन) और (ii) दुर्बल वचन (कम प्रभावशाली कथन)। तर्कशास्त्र में प्रबल वचन को सिद्धांत वचन कहा जाता है, जो अंतिम सत्य को व्यक्त करता है, जबकि दुर्बल वचन को पूर्व पक्ष वचन कहा जाता है, जिसे आगे जाकर खंडित किया जाता है। अधिक प्रभावशाली और निर्णायक वचन कम प्रभावशाली वचनों को निरस्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए, "अहिंसा परमो धर्मः" (अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है) यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शास्त्र-वचन है, लेकिन इससे भी अधिक प्रभावशाली वचन है—"यज्ञे पशवो वध्याः" (यज्ञ में पशुओं का वध किया जाना चाहिए), जो विशेष परिस्थितियों में अहिंसा के सामान्य नियम को निरस्त करता है।
इसी प्रकार, "कर्मफलम् अवश्यं अनुभवनीयम्" (कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है) यह कथन भी तब अपनी महत्ता खो देता है जब उससे अधिक प्रभावशाली कथन "तपसा किल्बिषं हंति" (तप से पाप नष्ट होते हैं, मनु स्मृति XII-104) आता है। अतः जन्म-जन्मांतर के संचित पुण्य-पाप रूपी कर्म, चाहे वे कितने भी विशाल हों, आत्मज्ञान द्वारा पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं।
संक्षेप में, बिना कर्म के पुनर्जन्म नहीं होता; बिना पुनर्जन्म के दुख नहीं होता; और जब दुख समाप्त हो जाता है, तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। यही वेदांत का अंतिम निष्कर्ष है।
वर्णक 5
बंधन की श्रृंखला II – कर्म, प्रेम और घृणा
पूर्व अध्याय में यह बताया गया कि जीव की पीड़ाएँ केवल शरीर के साथ जुड़ाव के कारण हैं, और यह शरीर कर्मों का परिणाम है।
संदेह: कर्म कितने प्रकार के होते हैं?
स्पष्टीकरण: कर्म तीन प्रकार के होते हैं— (i) पुण्य (सत्कर्म), (ii) पाप (दुष्कर्म) और (iii) मिश्रित (पुण्य और पाप दोनों का सम्मिश्रण)। देवता आदि के शरीर पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं, पशु आदि के शरीर पाप कर्मों के कारण मिलते हैं और मनुष्यों के शरीर मिश्रित कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। प्रत्येक प्रकार के कर्मों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है— (i) उत्कृष्ट (श्रेष्ठ), (ii) मध्यम (मध्यम) और (iii) सामान्य (सामान्य)। इन विविध प्रकार के कर्मों के कारण अनेक प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं।
संदेह: विभिन्न प्रकार के पुण्य, पाप और मिश्रित कर्मों के परिणाम क्या होते हैं?
स्पष्टीकरण: उत्कृष्ट पुण्य कर्मों (अत्यधिक उत्तम पुण्य कर्म)
के कारण हिरण्यगर्भ (सृष्टि के
अधिष्ठाता) और अन्य देवताओं के
शरीर प्राप्त होते हैं। मध्यम
पुण्य कर्मों के कारण इंद्र
आदि देवताओं के शरीर प्राप्त
होते हैं। सामान्य पुण्य कर्मों के कारण
यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के
शरीर प्राप्त होते हैं।
उत्कृष्ट पाप कर्मों
(अत्यधिक घोर पाप)
के कारण ऐसे शरीर प्राप्त
होते हैं जो दूसरों को
हानि पहुँचाते हैं,
जैसे—काँटेदार या विषैले वृक्ष,
बाघ, साँप, बिच्छू,
उल्लू, मच्छर, जोंक आदि। मध्यम
पाप कर्मों के कारण ऐसे
पेड़-पौधे और जीव मिलते
हैं, जो मनुष्यों के लिए कुछ हद
तक उपयोगी होते हैं, जैसे कटहल,
आम, केला, नारियल आदि के
वृक्ष तथा सुअर,
भैंस, गधा, ऊँट आदि। सामान्य
पाप कर्मों के कारण पीपल,
तुलसी, बेल आदि वृक्ष तथा
गाय, घोड़े आदि के शरीर
प्राप्त होते हैं।
उत्कृष्ट मिश्रित कर्मों
(श्रेष्ठ मिश्रित कर्म)
के कारण ऐसे मनुष्य जन्म
लेते हैं, जो निष्काम कर्म
में स्थित होते हैं, जिन्हें सद्गुरु प्राप्त होता है और
जो श्रवण, मनन,
आत्म-ज्ञान और जीवनमुक्ति के
मार्ग से परम मुक्ति प्राप्त
करते हैं। मध्यम मिश्रित कर्मों
के कारण वे मनुष्य जन्म
लेते हैं, जो अपने वर्ण
और आश्रम के अनुसार कर्तव्यों का पालन
करते हैं, परन्तु इन कर्मों
के फलों की कामना भी
रखते हैं। सामान्य मिश्रित कर्मों के परिणामस्वरूप चांडाल, शिकार करने वाले, अत्याचारी और अन्य घृणित
जीवन जीने वाले मनुष्यों का
जन्म होता है।
अतः विवेकवान व्यक्ति को पहले यह विचार
करना चाहिए कि उसके कर्म
किस प्रकार के फल देंगे।
उसे केवल उन्हीं कर्मों को
अपनाना चाहिए जो उसे श्रेष्ठ
मानव जीवन की ओर ले
जाएँ और अंततः आत्मज्ञान के
माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कराएँ।
संदेह: इन तीनों प्रकार के कर्मों को कौन करता है?
स्पष्टीकरण: ये कर्म तीन साधनों (करणों) द्वारा किए जाते हैं— (i) मन (मनस), (ii) वाणी (वाक्), और (iii) शरीर (काय)।
संदेह: संसार में लोग "मैं करता हूँ", "मैं करता हूँ" इस प्रकार के वाक्य कहते हैं। इससे प्रतीत होता है कि 'मैं' जो आत्मा है, वही कर्ता है। तो फिर कर्म का संबंध इन तीन साधनों से कैसे जोड़ा जाता है?
स्पष्टीकरण: आत्मा तो अपरिवर्तनशील, निष्क्रिय और अद्वैत स्वरूप है, इसलिए उसमें कर्तृत्व भाव नहीं हो सकता।
संदेह: फिर ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आत्मा ही कर्ता है, जबकि कोई अन्य कर्ता दिखाई नहीं देता?
स्पष्टीकरण: आत्मा में कर्तृत्व का बोध केवल अध्यास (अज्ञानजनित भ्रम) के कारण होता है, यह उसका स्वाभाविक गुण नहीं है। यदि यह उसका स्वाभाविक गुण होता, तो लोग यह प्रयास ही न करते कि "मेरे भीतर के कर्तापन के झूठे भाव को वेदांत अध्ययन के द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी।"
संदेह: मान लिया जाए कि कर्तृत्व आत्मा का स्वाभाविक गुण है, तो क्या उसे नष्ट करने का प्रयास नहीं किया जा सकता?
स्पष्टीकरण: नहीं, क्योंकि जो स्वाभाविक होता है, वह व्यक्ति की स्वयं की वास्तविकता होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रकृति को नष्ट करने का प्रयास नहीं करता। यदि आत्मा की मूल प्रकृति नष्ट हो जाए, तो फिर आत्मसाधना का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। यदि जीवन्मुक्त अवस्था (शरीर में रहते हुए मुक्ति) को नकार दिया जाए, तो गुरु-शिष्य परंपरा जैसी संपूर्ण वेदांत परंपरा भी व्यर्थ हो जाएगी। इसके अलावा, श्रुतियों में कहा गया है कि "आत्मा निष्कल (अखंड), निष्क्रिय, शांत, निर्दोष और निर्मल है" (श्वेताश्वतर उपनिषद VI-19)। अतः यह स्पष्ट है कि आत्मा में कर्तृत्व का गुण प्राकृतिक रूप से नहीं है, यह केवल अज्ञानजनित भ्रांति (अध्यास) का परिणाम है।
संदेह: यदि आत्मा स्वप्न और जाग्रत अवस्था में कर्ता प्रतीत होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि गहरी निद्रा (सुषुप्ति) में कर्तृत्व प्रकट न हो, क्योंकि वहां साधनों की अनुपस्थिति होती है? जैसे कोई बढ़ई जब स्नान या भोजन कर रहा होता है, तब उसके औज़ार न होने के कारण कारीगरी प्रकट नहीं होती।
स्पष्टीकरण: ऐसा नहीं है। आत्मा जब पूर्ण रूप से शांत होती है, तब भी कर्तृत्व प्रकट नहीं होता। यह प्रमाणित करता है कि आत्मा में कर्तृत्व का गुण स्वाभाविक रूप से नहीं है, बल्कि यह केवल अध्यास (भ्रम) का परिणाम है।
संदेह: अध्यास (अज्ञानजनित भ्रम) क्या है?
स्पष्टीकरण: अध्यास का अर्थ है किसी वस्तु के गुणों को दूसरी वस्तु में देखना। जैसे जब कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी में चलता है, तो किनारे के वृक्ष उसे हिलते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ नाव की गति वृक्षों में आरोपित कर दी जाती है और वृक्षों की स्थिरता नाव पर आरोपित कर दी जाती है। इसी प्रकार मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सभी कर्मों को आत्मा में आरोपित कर दिया जाता है, और आत्मा की निष्क्रियता इन साधनों पर आरोपित कर दी जाती है। यह केवल अज्ञान के कारण होता है। अतः यह समझना चाहिए कि आत्मा में कर्तृत्व की कल्पना केवल अध्यास का परिणाम है।
संदेह: यदि कर्म के साधन (मन, वाणी, शरीर) जड़ और अचेतन हैं, तो उनमें कर्तृत्व (कर्तापन) कैसे हो सकता है? यदि वे स्वयं कर्ता होते, तो उन्हें भी क्रियाशील करने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता होती। यदि ऐसा है, तो वे अन्य साधन क्या हैं?
स्पष्टीकरण: यह आवश्यक नहीं है कि जड़ साधनों को सक्रिय करने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, हवा और बाढ़ जैसी जड़ शक्तियाँ बिना किसी अन्य बाहरी साधन के वृक्षों को उखाड़कर दूर ले जाती हैं। इसी प्रकार, मन, वाणी और शरीर बिना किसी अन्य साधन के कर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं।
संदेह: मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए कर्म कौन-कौन से होते हैं?
स्पष्टीकरण:
● मन के पुण्य कर्म: सत्कल्प, उच्च आध्यात्मिक विचार, परलोक चिंतन आदि।
● मन के पाप कर्म: विषयासक्ति, दूसरों के प्रति द्वेष, शास्त्रों पर संदेह, पाप-पुण्य में भेद न मानना आदि।
● मन के मिश्रित कर्म: सत्कर्मों के साथ-साथ सांसारिक सुख की इच्छा रखना।
● वाणी के पुण्य कर्म: वेदों का अध्ययन, जप, सत्संग, सत्य वचन, मधुर और विनम्र वाणी आदि।
● वाणी के पाप कर्म: झूठ, निंदा, कठोर वचन, निरर्थक बातें करना आदि।
● वाणी के मिश्रित कर्म: पूजा-पाठ के दौरान सांसारिक विषयों पर चर्चा करना।
● शरीर के पुण्य कर्म: तीर्थ स्नान, गुरु और देवताओं को प्रणाम, समाज-सेवा आदि।
● शरीर के पाप कर्म: हिंसा, चोरी, व्यभिचार, बुरे लोगों की संगति आदि।
● शरीर के मिश्रित कर्म: धर्मार्थ कार्य के लिए अन्यायपूर्ण साधनों का उपयोग करना।
इन तीनों प्रकार के कर्मों का गहराई से विचार किया जाना चाहिए।
संदेह: ऐसे जिज्ञासा करने का क्या लाभ है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
स्पष्टीकरण:
इस प्रकार की जिज्ञासा का
परिणाम दो प्रकार का होता
है— (i) मुख्य
फल और (ii) अवांतर फल। जैसा
कि पहले कहा गया है,
तीन प्रकार के कर्म केवल
तीन साधनों (मन,
वाणी और शरीर)
द्वारा किए जाते हैं। आत्मा
इनसे अछूती होती है और
आकाश की भांति विभाजन रहित
होती है। यह स्वयं चेतना-स्वरूप है। इसलिए
यह किसी भी प्रकार के
कर्म की कर्ता नहीं हो
सकती, जैसा कि शास्त्रों में
कहा गया है:
"जो आत्मा स्वप्न में अनुभव
करता है, जाग्रत अवस्था में
भोगता है, फिर भी अपने
शाश्वत स्वरूप में स्थित रहता
है, वही वास्तविक आत्मा है।"
इसका तात्पर्य यह है कि
आत्मा न तो किसी कर्म
से प्रभावित होती है और
न ही किसी प्रकार का
कार्य करती है। जब यह
समझ लिया जाता है कि
"चिदाकाशस्वरूप आत्मा
किसी भी कर्म से स्पर्श
नहीं करती", तब व्यक्ति सभी
शंकाओं को त्यागकर गहन शांति और संतोष
प्राप्त करता है। यही इसका
मुख्य लाभ है।
इसके अतिरिक्त, ब्रह्म-ज्ञान प्राप्ति के
बाद भी व्यक्ति को अपने तीन साधनों
(मन, वाणी, शरीर)
को पुण्य कर्मों में लगाना
चाहिए। यदि यह संभव न
हो, तो कम से कम
मिश्रित कर्म करने चाहिए, किंतु पाप कर्मों की
ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार जीवन के इस
नियम को समझकर उसमें स्थित
रहना ही इस जिज्ञासा का
द्वितीयक लाभ है। इसे एक
उदाहरण से समझ सकते हैं—
जैसे केले के वृक्ष को
उगाने वाले व्यक्ति के लिए उसका फल
मुख्य लाभ होता है, जबकि उसके पत्ते, फूल आदि गौण लाभ
होते हैं।
संदेह: क्या ज्ञानी पुरुष वास्तव में कर्मों से अछूते होते हैं, जैसे जल से कमल पत्र? यदि यह सिद्ध हो गया है कि वे अकर्ता (कर्तृत्व से रहित) हैं और केवल साक्षी मात्र हैं, तो फिर उनके लिए भी पुण्य कर्म करने का नियम क्यों आवश्यक बताया गया है?
स्पष्टीकरण: हाँ, इसमें कोई संदेह
नहीं कि ज्ञानी पुरुष को
कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती,
और वे किसी भी कर्म
के कर्ता नहीं होते। फिर
भी, ज्ञानी पुरुष चार प्रकार
के होते हैं—
(i) ब्रह्मवित (ब्रह्म को जानने वाला),
(ii) ब्रह्मविद्वर (श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी), (iii) ब्रह्मविद्वरियन (अधिक श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी) और
(iv) ब्रह्मविद्वरिष्ठ (सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी)। इनमें
से केवल ब्रह्मविद्वरिष्ठ ही विदेहमुक्त होते हैं,
अर्थात वे पूर्ण रूप से
चित्तवृत्तियों से
मुक्त होते हैं। उनके लिए
किसी भी प्रकार के नियम-निषेध लागू नहीं
होते।
शेष तीन प्रकार के ज्ञानी
पुरुष, यद्यपि वे भी नियमों
से परे होते हैं, फिर भी वे उचित
आचरण का पालन करते हैं।
क्योंकि वे अभी भी मानसिक
वृत्तियों से पूर्णतः मुक्त नहीं हुए होते,
संसार में क्रियाशील रहते हैं और लोक
कल्याण के कार्यों में संलग्न होते हैं।
अतः वे समाज में एक
आदर्श प्रस्तुत करने हेतु पुण्य
कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। परंतु आध्यात्मिक साधकों के
मध्य वे सभी कर्मों का
त्याग करके केवल ज्ञान की
सर्वोच्चता की घोषणा करते हैं:
"ब्रह्म सत्यं,
अन्यत् सर्वं असत्यं"—"केवल ब्रह्म ही
सत्य है, बाकी सब मिथ्या
है।"
अतः यह स्पष्ट है कि
कर्तृत्व केवल मन,
वाणी और शरीर में स्थित
होता है, न कि आत्मा
में।
संदेह: क्या ये तीन साधन (मन, वाणी, शरीर) स्वयं ही कार्य करते हैं या कोई बाहरी शक्ति इन्हें प्रेरित करती है?
स्पष्टीकरण: गहन विचार करने पर ज्ञात होता है कि ये साधन स्वयं नहीं चलते, बल्कि राग और द्वेष जैसी भावनाओं के प्रभाव में कार्य करते हैं। अनुभव द्वारा भी इसे समझा जा सकता है— जब राग, द्वेष आदि की भावना उत्पन्न होती है, तो ये साधन कार्य करते हैं, और जब ऐसी भावनाएँ नहीं होतीं, तो वे निष्क्रिय रहते हैं।
संदेह: जब लोग कहते हैं, "मैं मंदिर बनवा रहा हूँ", "मैं तालाब खुदवा रहा हूँ", तो क्या यह प्रमाणित नहीं होता कि आत्मा प्रेरक कर्ता है, भले ही वह प्रत्यक्ष कर्ता न हो?
स्पष्टीकरण: नहीं। आत्मा चूँकि अपरिवर्तनशील है, इसलिए वह कर्मों की प्रेरक शक्ति नहीं हो सकती।
संदेह: फिर आत्मा में यह कर्तृत्व का भाव कैसे प्रतीत होता है?
स्पष्टीकरण:
यह केवल भ्रम
(मिथ्या धारणा) के कारण होता
है। जैसे जब लाल जवा
पुष्प का प्रतिबिंब एक स्वच्छ स्फटिक में
पड़ता है, तो देखने में
लगता है कि स्फटिक स्वयं
लाल रंग का हो गया
है, वैसे ही राग-द्वेष आदि के कारण
उत्पन्न होने वाले कर्म आत्मा
में आरोपित कर दिए जाते
हैं। यदि आत्मा में कर्तृत्व का गुण
स्वाभाविक होता, तो कोई भी
व्यक्ति इसे समाप्त करने का
प्रयास न करता। जो स्वाभाविक होता है,
वही वास्तविकता होती है, और यदि उस स्वाभाविकता का नाश
किया जाए, तो स्वयं की
वास्तविकता भी नष्ट हो जाएगी।
यदि आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक होता, तो शास्त्रों में कहा गया यह
वचन— "अदृश्यं,
अग्रह्यं, अलक्षणं, अचिन्त्यम्, अव्यपदेश्यम्, एकात्मप्रत्ययसारं, प्रपंचोपशमं, शान्तं, शिवं, अद्वैतं"
(माण्डूक्य उपनिषद् 7)— कि आत्मा असंग,
अकर्ता और निर्लेप है, असत्य सिद्ध हो
जाता। इसके अतिरिक्त, यदि आत्मा
की प्रेरक शक्ति स्वाभाविक होती,
तो मुक्ति भी किसी कर्म
का परिणाम होती,
और यदि मुक्ति कर्म का
परिणाम होती, तो वह भी
नष्ट होने योग्य होती। किंतु
ऐसा नहीं है। अतः आत्मा
का प्रेरक होना उसकी स्वाभाविक प्रकृति नहीं,
बल्कि केवल बाहरी संयोग (अविद्या) के कारण प्रतीत
होता है।
संदेह: केवल यह देखकर कि गहरी निद्रा (सुषुप्ति) में कर्तृत्व नहीं पाया जाता, क्या यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि आत्मा प्रेरक नहीं है? उदाहरण के लिए, एक शिक्षक में उसकी शिक्षण क्षमता बनी रहती है, भले ही वह विद्यार्थियों के अनुपस्थित होने पर शिक्षण न कर रहा हो। उसी प्रकार, आत्मा में प्रेरक शक्ति बनी रहती होगी, परंतु निद्रा में केवल साधनों के अभाव के कारण वह दिखाई नहीं देती। क्या यह तर्क उचित नहीं है?
स्पष्टीकरण:
यदि यह तर्क स्वीकार कर
लिया जाए, तो निष्क्रियता, तटस्थता आदि जैसी अवस्थाओं में, जो जाग्रत अवस्था में
ही होती हैं,
आत्मा को प्रेरक शक्ति के
रूप में कार्यरत रहना चाहिए,
क्योंकि उन अवस्थाओं में भी आत्मा अपने
साधनों से जुड़ी रहती है।
किंतु ऐसा नहीं होता। अतः
यह सिद्ध होता है कि
आत्मा की प्रेरक शक्ति केवल
बाह्य कारणों से उत्पन्न हुई
एक कल्पना मात्र है, न कि उसकी मूल
प्रकृति।
इस सिद्धांत को और अधिक
स्पष्ट करने के लिए एक
उदाहरण लेते हैं—
जब एक लोहे की छड़
को लाल गरम किया जाता
है, तो उसमें आग के
गुण (गर्मी और प्रकाश) आ जाते हैं, और आग में लोहे
के गुण (ठोसता)
का आरोप हो जाता है।
यह गुणों का आपसी स्थानांतरण है। इसी
प्रकार, आत्मा में कर्तृत्व का
आरोप राग, द्वेष आदि के
कारण होता है,
और राग-द्वेष आदि में
आत्मा की निर्लेपता का आरोप हो जाता
है। यह केवल अज्ञान (अविद्या) के कारण होने
वाली गलत धारणा है।
संदेह: फिर निष्क्रिय राग और द्वेष कैसे कर्म का कारण बन सकते हैं? क्या यह कहना उचित होगा कि एक मिट्टी का घड़ा दूसरे घड़े को क्रियाशील बना सकता है?
स्पष्टीकरण: यह सच है कि राग और द्वेष स्वयं जड़ (निष्क्रिय) हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब जड़ पदार्थ अन्य तत्वों के संपर्क में आते हैं, तो वे क्रियाशील हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आग अपने आप में जड़ है, लेकिन जब यह गंधक और लकड़ी के कोयले के मिश्रण से बने बारूद के संपर्क में आती है, तो यह इतनी तीव्र गति से गोलियां दाग सकती है कि दूर स्थित सेनाओं को नष्ट कर दे। इसी प्रकार, एक मृत शरीर स्वयं जड़ होते हुए भी अपने रिश्तेदारों को उसकी अंतिम क्रियाएँ करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह, राग-द्वेष आदि, यद्यपि जड़ हैं, फिर भी वे प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं।
संदेह: फिर शास्त्रों में जो यह कहा गया है कि "आत्मा इंद्रियों का स्वामी और सभी प्राणियों में आंतरिक शासक है", इसका क्या अर्थ है?
स्पष्टीकरण: जैसे सूर्य मात्र अपनी उपस्थिति से संसार के सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कार्यों को संपन्न होने देता है, लेकिन स्वयं उन कार्यों से अप्रभावित रहता है, वैसे ही आत्मा भी है। जैसे चुम्बक की उपस्थिति मात्र से लोहे को गति मिलती है, लेकिन स्वयं चुम्बक उस गति से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार सभी प्राणियों के कर्म आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा सदा पवित्र और अपरिवर्तनशील बनी रहती है।
संदेह: यदि गुरु द्वारा आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट रूप से बताया जाता है, तो भी शिष्य के मन में दृढ़ विश्वास क्यों नहीं उत्पन्न होता?
स्पष्टीकरण: यह तीन प्रकार की
बाधाओं (प्रतिबंधकों) के कारण होता
है— (i) संशय
भावना (संदेह), (ii) असंभवता भावना (असंभव लगना), और (iii) विपरीत भावना (उल्टा अनुभव होना)। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार
(जनेऊ धारण करना)
का उल्लेख ऋग्वेद में अलग-अलग तरीकों से
किया गया है,
वैसे ही विभिन्न शास्त्रों में अद्वैत आत्मा
के बारे में विभिन्न प्रकार
की व्याख्याएँ दी गई हैं।
यदि कोई व्यक्ति यह संदेह करता है
कि "क्या
आत्मा एक है या अनेक?",
तो यह संशय भावना कहलाती
है। इस संदेह को दूर
करने के लिए बार-बार शास्त्रों के श्रवण
(सुनने) की आवश्यकता होती है। लेकिन यह
प्रक्रिया केवल एक प्रकार के
संदेह, जिसे प्रमाणगत संशय कहते हैं, को नष्ट कर सकती
है।
श्रवण करने के बाद व्यक्ति
इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता
है कि "सभी वेदांत ग्रंथ
एक ही अद्वैत ब्रह्म की
बात करते हैं",
लेकिन फिर भी उसे यह
संदेह हो सकता है कि
"जीव, ईश्वर और जगत स्पष्ट
रूप से अलग-अलग प्रतीत होते
हैं, तो अद्वैत ब्रह्म की
स्थिति संभव कैसे हो सकती
है?" इसे
असंभवता भावना कहते हैं। इसे
दूर करने के लिए व्यक्ति
को मनन (तर्क द्वारा विचार)
करना पड़ता है,
जैसे स्वप्न में देखे गए
अनुभवों का विश्लेषण करके।
लेकिन यदि श्रवण और मनन
करने के बावजूद संसार वास्तविक लगता है
और आत्मा का ज्ञान दृढ़
नहीं होता, तो यह विपरीत
भावना के कारण होता है।
इसे दूर करने के लिए
निदिध्यासना (अखंड ध्यान)
की आवश्यकता होती है, जिसमें आत्मा के विचारों
की एक अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती है।
संदेह: जब ज्ञान के द्वारा सीधा आत्म-साक्षात्कार किया जा सकता है, तो फिर इन बाधाओं को दूर करने के लिए इतना परिश्रम क्यों करना चाहिए?
स्पष्टीकरण:
यह सच है कि ज्ञान
आत्म-साक्षात्कार में सहायक होता
है, लेकिन जब तक यह
ज्ञान इन तीन बाधाओं से
मुक्त नहीं होता,
तब तक यह प्रभावी नहीं
हो सकता। उदाहरण के लिए,
अग्नि में सभी चीजों को
जलाने की शक्ति होती है,
लेकिन यदि किसी विशेष मंत्र
या तंत्र द्वारा इसे बांध
दिया जाए, तो यह एक
तिनके को भी नहीं जला
सकती। इसी प्रकार,
ज्ञान में अज्ञान और उसके
प्रभावों को तुरंत नष्ट करने
की क्षमता होती है, लेकिन जब तक यह
तीन बाधाओं से घिरा होता
है, तब तक यह प्रभावी
रूप से कार्य नहीं कर
सकता।
एक बार जब ये तीनों
बाधाएँ नष्ट हो जाती हैं,
तो ज्ञान तुरंत अज्ञान को
जला देता है,
जैसे सूखी घास को अग्नि
तुरंत भस्म कर देती है।
यहां इस संबंध में याद रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अध्ययन के योग्य किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ के वास्तविक अभिप्राय को समझने के लिए षड्लिंग या प्रमाण के छह साधनों की सहायता लेनी चाहिए। क्योंकि यह कहा गया है कि 'उपक्रम-उपासंहार (आरंभ और निष्कर्ष में एक ही विषय का प्रतिपादन), अभ्यास (दोहराव), अपूर्वता (विशिष्टता), फल (लाभ), अर्थवाद (स्तुति) और उपपत्ति (तार्किक प्रमाण) - ये छह प्रमाण किसी भी ग्रंथ के वास्तविक अभिप्राय को निर्धारित करने के साधन हैं।' इस कथन के अनुसार, इन छह साधनों को किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ के वास्तविक अभिप्राय के निर्धारण में कठोरता से अपनाया जाना चाहिए।
षड्लिंग को निम्नलिखित प्रकार से समझाया गया हैः
1. उपक्रम-उपासंहार – छांदोग्य उपनिषद
में छठे अध्याय की शुरुआत
इस वाक्य से होती है,
'प्रारंभ में केवल सत्य ही
था, एक और अद्वितीय' (VI-ii-1), और
इस विषय का निष्कर्ष अखंड
एकरसता या एक अविभाज्य समरूप
तत्व की पुष्टि करते हुए
इस कथन के साथ किया
जाता है—'यह सब उसी
की प्रकृति है;
वही सत्य है'
(VI-viii-7)। इस
प्रकार, जब आरंभ और निष्कर्ष में एक
ही विषय का प्रतिपादन हो,
तो वह ग्रंथ के मुख्य
अभिप्राय को समझने में सहायक
होता है। यही उपक्रम-उपासंहार की उपयोगिता है।
2. अभ्यास
– इसी उपनिषद में महान वाक्य
"तत् त्वम् असि"
(VI-viii-7) का नौ
बार दोहराव किया गया है।
यह पुनरावृत्ति अभ्यास प्रमाण कहलाती
है।
3. अपूर्वता
– इस ग्रंथ का मुख्य विषय,
अर्थात् 'अखंड समरूप तत्व', प्रत्यक्ष आदि सामान्य प्रमाणों की सीमा
से परे है। दूसरे शब्दों
में, इसे सामान्य ज्ञान-साधनों द्वारा नहीं
जाना जा सकता। इस विषय
की यह विशेषता या अनूठापन अपूर्वता कहलाती है।
4. फल
– इसी ग्रंथ में कहा गया
है, 'जब तक उसे मोक्ष
प्राप्त नहीं होता,
तब तक उसे यहीं रहना
होगा; फिर वह अपने वास्तविक स्वरूप को
प्राप्त करता है'
(VI-xiv-2)। यह
स्पष्ट करता है कि अखंड
समरूप तत्व के ज्ञान से
प्राप्त लाभ परम मोक्ष, अर्थात् देह त्याग के
बाद विदेहमुक्ति है। यही फल
प्रमाण है।
5. अर्थवाद
– यह प्रशंसा या स्तुति होती
है, जिसे आगे विस्तार से
समझाया गया है।
6.
उपपत्ति – उपनिषद का यह वचन,
'जिस प्रकार मृत्तिकामय वस्तुओं को केवल मृत्तिका को जानकर
ही जाना जा सकता है'
(छांदोग्य उपनिषद VI-i-4), मुख्य विषय को
तार्किक रूप से स्पष्ट करता
है। यह तार्किक व्याख्या उपपत्ति कहलाती है।
अर्थवाद या
स्तुति के सात प्रकार होते
हैंः
(i) सृष्टि (उत्पत्ति), (ii) स्थिति
(संरक्षण), (iii) प्रलय
(संहार), (iv) प्रवेश
(अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होना),
(v) संयमन (नियंत्रण), (vi) तत् त्वम् पदार्थ
परिशोधन (महावाक्य 'तत् त्वम् असि'
का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करना),
और (vii) फल
(लाभ)।
शास्त्रों में 'वास्तव में आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ' (तैत्तिरीय उपनिषद II-1) आदि वाक्य ब्रह्म को सृष्टिकर्ता रूप में प्रशंसित करते हैं। ये हमें यह भी सिखाते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के घड़े आदि अपने उत्पत्ति स्रोत, आधार और संहार में मिट्टी से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार आकाश आदि, जो ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, उसमें स्थित रहते हैं और अंततः उसमें विलीन हो जाते हैं। अतः वे वास्तव में ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ऐसे वाक्य महावाक्य 'तत् त्वम् असि' द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत को स्थापित करते हैं। ये सृष्टि, स्थिति और प्रलय रूपी तीन अर्थवाद हैं।
फिर, 'उसने सिर के शीर्ष को भेदकर इस छिद्र से प्रवेश किया' (ऐतरेय उपनिषद I-iii-12), 'आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया' (तैत्तिरीय उपनिषद II-6), 'इन जीवों में प्रवेश करके, मैं नाम और रूप की सृष्टि करूं' (छांदोग्य उपनिषद VI-iii-2) आदि वाक्य, जो यह बताते हैं कि ब्रह्म ने जीव के रूप में शरीर में प्रवेश किया है, जीव और ब्रह्म की अभिन्नता को प्रमाणित करते हैं। यह 'प्रवेश' प्रमाण है।
संयमन का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। उपनिषद का वचन, 'जो पृथ्वी में स्थित है, जो पृथ्वी को नियंत्रित करता है, परंतु पृथ्वी जिसे नहीं जानती, वही तेरा आत्मा, आंतरिक शासक, अमर है' (बृहदारण्यक उपनिषद III-vii-3), आदि, जो ब्रह्म के नियंत्रक स्वरूप को दर्शाते हैं, इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि नियंत्रक आत्मा और नियंत्रित अ-आत्मा में भेद मात्र प्रतीतिभासिक है।
तत् त्वम् पदार्थ परिशोधन – जो शास्त्रीय वचन महावाक्य 'तत् त्वम् असि' के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, वे ईश्वर और जीव की एकता को स्थापित करते हैं, उनके परस्पर विरोधी गुणों को निषेध करके। जैसे, 'निश्चय ही यह आत्मा अन्नरस का सार है' (तैत्तिरीय उपनिषद I-1), 'लालिमा अग्नि का रंग है' (छांदोग्य उपनिषद VI-iv-1) आदि।
फल – इस अद्वैत ज्ञान से प्राप्त होने वाले अद्भुत फल को प्रकट करने वाले शास्त्रीय वाक्य, जैसे 'ब्रह्म को जानने वाला परम पद को प्राप्त करता है' (तैत्तिरीय उपनिषद II-1), 'वह अमर हो गया' (ऐतरेय उपनिषद III-4), न केवल इस एकता को घोषित करने की इच्छा को प्रकट करते हैं, बल्कि इसे स्थापित भी करते हैं।
चूंकि महावाक्य 'तत् त्वम् असि', अपने सहायक वचनों के साथ, अखंड समरूप तत्व को प्रतिपादित करता है, और यह सात प्रकार के अर्थवाद द्वारा समर्थित है, इसका अर्थ शिष्य को इस अविभाज्य समरूप तत्व के रूप में सिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार, शास्त्रों के उद्देश्य का निर्धारण, जैसा कि उपर्युक्त षड्लिंग प्रमाणों से किया गया है, श्रवण (शास्त्रों का सुनना) कहलाता है।
अब हम अपने मुख्य विषय पर लौटते हैं। इस अध्याय में विवेचित प्रेरणात्मकता के स्वरूप की जांच करने के बाद, व्यक्ति को इस अटल निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए—'राग, द्वेष आदि के प्रभाव से तीन साधन (मन, वचन, कर्म) तीन प्रकार की क्रियाओं को करते हैं। जैसे राजा युद्ध की विजय का श्रेय स्वयं लेता है, जबकि वास्तव में सेना, जो सेनापति द्वारा संचालित होती है, विजय प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा स्वयं को प्रेरक मान लेता है, जबकि वास्तविक प्रेरणात्मकता राग, द्वेष आदि में निहित होती है। किंतु आत्मा में न तो कर्तृत्व है, न प्रेरणात्मकता।' इस अटल समझ वाला व्यक्ति ही जीवनमुक्त कहलाता है।
वर्णक -6
बंधन की श्रृंखला III –
प्रेम और घृणा, आत्म-परिचय, अविवेक और अज्ञान
बंधन की श्रृंखला' के सात कड़ियों में से, हमने पहले चार पर विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि एक दूसरे का कारण बनती है। इस छठे अध्याय में राग-द्वेष (प्रेम और घृणा), अभिमान (शरीर आदि के साथ तादात्म्य), अविवेक (विवेक का अभाव) और अज्ञान (अविद्या) की विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया जाएगा।
मानसिक विकार सोलह प्रकार के होते हैं। वे हैं— (1) राग (प्रेम), (2) द्वेष (घृणा), (3) काम (इच्छा), (4) क्रोध (रोष), (5) लोभ (कृपणता), (6) मोह (मोहग्रस्तता), (7) मद (अहंकारपूर्ण गर्व), (8) मत्सर्य (ईर्ष्या), (9) ईर्ष्या (असहिष्णुता), (10) असूया (द्वेषपूर्ण जलन), (11) दंभ (ढोंग), (12) दर्प (अहंकारपूर्ण घमंड), (13) अहंकार (स्वयं को प्रधान मानना), (14) इच्छा (अनिवार्य कार्य करने की प्रवृत्ति), (15) भक्ति (श्रद्धा और प्रेम), और (16) श्रद्धा (विश्वास)।
यौन सुखों के पीछे जो मानसिक विकार होता है, उसे राग कहा जाता है। मन की वह प्रवृत्ति जो बुराई का प्रतिशोध बुराई से लेने के लिए प्रेरित करती है, वह द्वेष कहलाती है। भूमि, घर आदि प्राप्त करने की तीव्र इच्छा काम है। ऐसे किसी भी अधिग्रहण में बाधा डालने वालों के प्रति उत्पन्न वितृष्णा क्रोध कहलाती है। अपनी अर्जित संपत्ति में से योग्य व्यक्तियों को एक कण भी न देने की प्रवृत्ति लोभ कहलाती है। संपत्ति के कारण उत्पन्न मोह के कारण क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस ज्ञान में रुचि न लेना या निषेधाज्ञाओं की अवहेलना करना मोह कहलाता है। 'मेरे पास अपार संपत्ति है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त न कर सकूं'— यह विचार मद कहलाता है। अपने समान स्थिति वाले किसी अन्य व्यक्ति को सहन न कर पाने की प्रवृत्ति मत्सर्य कहलाती है। 'यह दुख या कष्ट मुझे क्यों मिला, जबकि मेरे विरोधी को क्यों नहीं हुआ?'— यह भावना ईर्ष्या कहलाती है। 'यह आनंद या सुख केवल मुझे ही मिलना चाहिए; फिर इसे दूसरे कैसे भोग सकते हैं?'— यह भावना असूया कहलाती है। केवल नाम और प्रसिद्धि के लिए पुण्य कर्म करना दंभ कहलाता है। यह सोचना कि ‘मेरा कोई समकक्ष नहीं है’— दर्प कहलाता है। हर स्थिति और स्थान में अपनी प्रधानता को स्थापित करने की प्रवृत्ति अहंकार कहलाती है। भोजन करना, शौच करना आदि अनिवार्य कार्यों को करने की आवश्यकता का अनुभव करना इच्छा कहलाती है। गुरु, सत्पुरुषों और ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम और सम्मान भक्ति कहलाती है। कर्मकांडों की प्रभावशीलता में विश्वास, वेदांत के सिद्ध निष्कर्षों में आस्था और गुरु की शिक्षाओं में श्रद्धा रखना श्रद्धा कहलाता है। ये मन के सोलह प्रकार के विकार हैं।
संदेह: आत्मा के स्वरूप से संबंधित ग्रंथ में मानसिक विकारों की चर्चा करने का क्या उपयोग या आवश्यकता है?
स्पष्टीकरण: जीवों के मामले में बंधन और मोक्ष पूरी तरह से मन पर निर्भर होते हैं, न कि किसी अन्य वस्तु पर।
संदेह: यह कैसे?
स्पष्टीकरण: शुद्धता मन का मूल स्वभाव है। किंतु वह अशुद्ध वस्तुओं के संपर्क में आकर बंधन में पड़ गया है। मन का अपने मूल शुद्ध स्वरूप में स्थित होना ही मोक्ष कहलाता है। उपर्युक्त सोलह मानसिक विकारों में से पहले चौदह अशुद्ध हैं, किंतु अंतिम दो—भक्ति और श्रद्धा—शुद्ध हैं। राग से आरंभ होने वाले पहले तेरह विकार बिना किसी प्रयास के जीवों से बार-बार चिपक जाते हैं और उन्हें पापमय जीवन की ओर ले जाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए केवल पतन ही है, उत्थान नहीं। केवल वे ही व्यक्ति संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं, जो भक्ति और श्रद्धा रूपी शुद्ध मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होते हैं और मन की अशुद्ध प्रवृत्तियों को जीतने में सफल होते हैं।
इसलिए मनुष्य को अपने मन का निरंतर और गहन विश्लेषण करना चाहिए और राग आदि अशुद्ध प्रवृत्तियों को त्यागकर इसे भक्ति और श्रद्धा की दो उत्तम प्रवृत्तियों में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि राग आदि सदा अशुद्धि का कारण बनते हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि प्यास बुझाना, भूख मिटाना, प्राकृतिक क्रियाएं संपन्न करना आदि अनिवार्य कर्मों को टालना असंभव है। यदि कोई इन अनिवार्य कर्मों को छोड़ने का प्रयास करेगा, तो इससे और अधिक कष्ट ही होगा। ये कर्म न तो स्वर्ग की प्राप्ति का कारण बनते हैं और न ही नरक का। अतः भोजन ग्रहण करने आदि जैसे कार्य अनिवार्य रूप से करने चाहिए।
जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं में, जहाँ राग आदि मानसिक प्रवृत्तियाँ विद्यमान रहती हैं, वहाँ कर्म भी होते हैं। लेकिन गहरी निद्रा, मूर्छा, समाधि और योगियों की मौन अवस्था में राग आदि प्रवृत्तियाँ नहीं होतीं, अतः कर्म भी नहीं होते। इसलिए अन्वय और व्यतिरेक (सह-अस्तित्व और वियोग-अस्तित्व) की प्रक्रिया से यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि राग, द्वेष आदि ही कर्मों के कारण हैं।
संदेह: ये राग आदि कहाँ से उत्पन्न होते हैं?
स्पष्टीकरण: ये अभिमान (स्वरूप की गलत पहचान) से उत्पन्न होते हैं।
संदेह: क्या इसे उदाहरण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है?
स्पष्टीकरण: हाँ। उदाहरण के लिए, जब तक किसी स्त्री में यह अभिमान रहता है कि वह स्त्री है, तब तक प्रेम आदि भावनाएँ उसे पति की सेवा, गृहस्थी की देखभाल, भोजन बनाने आदि कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार, जब तक किसी पुरुष में पुरुष होने का अभिमान बना रहता है, तब तक वह विवाह, कृषि, व्यापार आदि कार्यों में प्रवृत्त रहता है। इसी तरह, सभी जीवों की विभिन्न गतिविधियाँ उनके अपने वर्णाश्रम या सामाजिक-धार्मिक अवस्थाओं से तादात्म्य रखने के कारण ही उत्पन्न होती हैं, और इस तादात्म्य का कारण राग आदि हैं। अतः इन सभी का मूल कारण केवल अभिमान ही है।
संदेह: तो इस विचार-विमर्श का लाभ क्या है?
स्पष्टीकरण: इसका लाभ यह है कि साधक को जाति, आश्रम, जीवन की विभिन्न अवस्थाएँ, जैसे बचपन, युवावस्था आदि, इन सबके प्रति अभिमान को त्याग देना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि यदि कोई अभिमान से मुक्त हो जाता है, तो वह बंधन से भी मुक्त हो जाता है। उसे अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा यह जानना चाहिए कि जहाँ अभिमान होता है, वहाँ राग, द्वेष आदि भी होते हैं, और जहाँ अभिमान नहीं होता, वहाँ राग, द्वेष आदि भी नहीं होते।
संदेह: यह कैसे?
स्पष्टीकरण: जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं में जाति और आश्रम आदि का अभिमान होने के कारण व्यक्ति राग आदि के माध्यम से कर्मों में प्रवृत्त रहता है। लेकिन गहरी नींद और अन्य समान अवस्थाओं में, जहाँ ऐसा कोई अभिमान नहीं होता, वहाँ राग आदि के कारण कोई कर्म भी नहीं होते।
संदेह: यदि ऐसा है, तो यह अभिमान कहाँ से उत्पन्न होता है?
स्पष्टीकरण: यह अविवेक (आत्मा और अनात्मा में भेद न कर पाना) से उत्पन्न होता है।
संदेह: यह कैसे?
स्पष्टीकरण: यद्यपि सभी व्यक्तियों का अस्तित्व उनके भौतिक शरीर से भिन्न होता है, फिर भी अविवेक के कारण उनमें अभिमान उत्पन्न हो जाता है, और वे सोचते हैं—'मैं ब्राह्मण हूँ', 'मैं क्षत्रिय हूँ', 'मैं वैश्य हूँ', 'मैं शूद्र हूँ', 'मैं ब्रह्मचारी हूँ', 'मैं गृहस्थ हूँ', 'मैं वानप्रस्थी हूँ', 'मैं संन्यासी हूँ', 'मैं पुरुष हूँ', 'मैं स्त्री हूँ' आदि। यही अविवेक अभिमान का कारण है, और कोई अन्य कारण नहीं।
संदेह: हम यह क्यों नहीं कह सकते कि शरीर ही अभिमान का कारण है, न कि अविवेक?
स्पष्टीकरण: यदि शरीर अभिमान का कारण होता, तो एक क्षत्रिय यह चेतना रख सकता था कि 'मैं ब्राह्मण हूँ', एक स्त्री यह मान सकती थी कि 'मैं पुरुष हूँ', एक ब्रह्मचारी यह सोच सकता था कि 'मैं गृहस्थ हूँ' आदि। लेकिन ऐसा कहीं भी देखा या सुना नहीं जाता। अतः अभिमान शरीर के आधार पर नहीं उत्पन्न होता।
संदेह: हम यह क्यों नहीं कह सकते कि ब्राह्मण होने का अभिमान उसके सिर पर जटाओं और यज्ञोपवीत के कारण उत्पन्न होता है, और संन्यासी का अभिमान उसके गेरुए वस्त्र, दंड और भिक्षा पात्र के कारण?
स्पष्टीकरण: नहीं; क्योंकि जटा और यज्ञोपवीत क्षत्रियों और यहाँ तक कि कुम्हारों में भी देखे जाते हैं। इसी प्रकार, गेरुआ वस्त्र आदि गैर-संन्यासियों में भी पाए जाते हैं। लेकिन इससे वे यह अनुभव नहीं करते कि 'मैं ब्राह्मण हूँ' या 'मैं संन्यासी हूँ'। इसलिए यह स्पष्ट है कि बाहरी भेदों के कारण अभिमान उत्पन्न नहीं होता।
संदेह: क्यों नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण होने का अभिमान विशेष शारीरिक लक्षणों के कारण उत्पन्न होता है, जैसे नर और नारी में प्राकृतिक भेद होते हैं?
स्पष्टीकरण: ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच ऐसे कोई विशिष्ट शारीरिक अंतर नहीं हैं।
संदेह: हम यह क्यों नहीं कह सकते कि अभिमान माता-पिता से प्राप्त शरीर के विशेष गुणों के कारण उत्पन्न होता है?
स्पष्टीकरण: यदि यह मान्यता सही होती, तो उनके बाल, नाखून, दाँत, मूत्र, मल आदि को भी 'ब्राह्मण' आदि का नाम दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए, भिन्न-भिन्न प्रकार के अभिमान केवल अविवेक के कारण उत्पन्न होते हैं, न कि किसी अन्य कारण से।
संदेह: इस अविवेक का कारण क्या है?
स्पष्टीकरण: अनादि अविद्या (प्रारंभहीन अज्ञान) ही अविवेक का कारण है। यह व्यक्ति के सच्चे स्वरूप को छिपा देती है और इसे केवल आत्मज्ञान से ही मिटाया जा सकता है। इसी अज्ञान के कारण व्यक्ति कहता है, 'मैं स्वयं को नहीं जानता।'
संदेह: यह कैसे संभव है? क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो स्वयं को नहीं जानता, सिवाय भ्रमित लोगों के?
स्पष्टीकरण: हाँ, इस संसार में ज्ञानी संतों को छोड़कर सभी लोग भ्रमित हैं।
संदेह: यह दुखद संसारिक अस्तित्व कब समाप्त होगा?
स्पष्टीकरण: जब शरीर का विनाश होता है, तो दुखों का भी विनाश हो जाता है। जब कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो शरीर का भी अंत हो जाता है। जब राग और द्वेष नष्ट हो जाते हैं, तो कर्म का भी नाश हो जाता है। अभिमान के समाप्त होने से राग-द्वेष समाप्त हो जाते हैं। अविवेक के विनाश से अभिमान का अंत होता है। अज्ञान के विनाश से अविवेक समाप्त हो जाता है। और यह अज्ञान उसी व्यक्ति में समाप्त हो जाता है, जो वेदों के महावाक्यों जैसे 'ब्रह्मैवाहमस्मि' ('ब्रह्म ही मैं हूँ') और 'अहं ब्रह्मास्मि' ('मैं ब्रह्म हूँ') से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में अडिग निश्चय रखता है और स्वयं को स्पष्ट रूप से आत्मा या ब्रह्म के रूप में पहचानता है। यह समझना चाहिए कि इस अज्ञान को नष्ट करने का कोई अन्य उपाय नहीं है।
संदेह: यह अज्ञान, जो तुच्छ और अवास्तविक ही है, कर्मों के प्रभाव से क्यों नहीं नष्ट हो सकता, जैसे कि ब्राह्मण हत्या जैसे जघन्य पाप भी उचित प्रायश्चित कर्मों के माध्यम से पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं?
स्पष्टीकरण: यह समझना चाहिए कि कर्म अज्ञान के विरोधी नहीं हैं; बल्कि वे इसे और बढ़ाते हैं। जिस प्रकार अमावस्या की रात में बादलों का घना पर्दा अंधकार को और अधिक गहरा कर देता है, वैसे ही कर्म अज्ञान को बढ़ाते हैं। डंडे से पीटना, तलवार से काटना, या उल्टा खड़े रहना—इनमें से कोई भी क्रिया अंधकार को दूर नहीं कर सकती; केवल प्रकाश ही अंधकार को मिटा सकता है। इसी प्रकार, कर्म अज्ञान को और गहरा करते हैं, न कि इसे मिटा सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी रात्रि के अंधकार को समाप्त करती है, उसी प्रकार केवल ज्ञान ही अज्ञान को मिटा सकता है, कर्म नहीं।
संदेह: कर्म तीन साधनों—मन, वाणी और शरीर—से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान भी अंतःकरण की एक मानसिक प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी एक कर्म ही होना चाहिए। फिर ज्ञान अज्ञान को कैसे नष्ट कर सकता है?
स्पष्टीकरण: यह सत्य है कि मानसिक प्रवृत्ति भी एक मानसिक क्रिया है। लेकिन यह प्रवृत्ति केवल अज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञान के लिए एक उपाधि (सहायक माध्यम) के रूप में कार्य करती है, जैसे भौतिक आँखें किसी वस्तु को देखने में सहायक होती हैं। स्वयं मानसिक प्रवृत्ति अज्ञान को नष्ट करने वाली नहीं है, बल्कि यह केवल ज्ञान की सहायता करती है। इसलिए, ज्ञान ही अज्ञान का नाश करने वाला तत्व है और यह शाश्वत है।
ज्ञान दो प्रकार का होता है—स्वरूप-ज्ञान (स्वाभाविक ज्ञान) और वृत्ति-ज्ञान (व्यवहारिक या प्रतिबिंबित ज्ञान)। यही स्वरूप-ज्ञान गहरी नींद में अज्ञान को प्रकाशित करता है और इसे ज्ञात कराता है। जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं में जो ज्ञान बाहरी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, वह वृत्ति-ज्ञान कहलाता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है: सूर्य की किरणें सीधे दीवार को प्रकाशित करती हैं। इस प्रकाश के ऊपर जब कई दर्पणों के माध्यम से सूर्य की किरणें फेंकी जाती हैं, तो दीवार पर अनेक बिंदुओं पर प्रकाश दिखाई देता है। इस स्थिति में, दोनों प्रकार के प्रकाश दीवार पर पड़ रहे होते हैं। इसी प्रकार, जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं में वृत्ति-ज्ञान, जो दर्पणों से परावर्तित प्रकाश के समान है, कार्य करता है; जबकि गहरी नींद में स्वरूप-ज्ञान, जो मूल सूर्यप्रकाश के समान है, विद्यमान रहता है।
संदेह: यदि ऐसा है, तो क्या यह निष्कर्ष निकाला जाए कि जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं में स्वरूप-ज्ञान मौजूद नहीं होता?
स्पष्टीकरण: नहीं। स्वरूप-ज्ञान हमेशा तीनों अवस्थाओं—जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—में विद्यमान रहता है। लेकिन वृत्ति-ज्ञान गहरी नींद की अवस्था में नहीं पाया जाता।
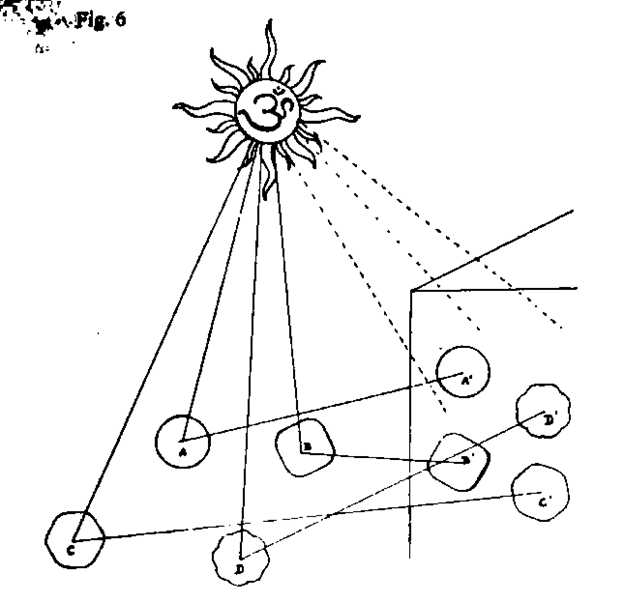
चित्र 6: स्वरूप-ज्ञान और वृत्ति-ज्ञान
आत्मा रूपी सूर्य की शाश्वत किरणें समस्त वस्तुओं को प्रकाशित कर रही हैं, यहाँ तक कि गहन निद्रा में व्याप्त अज्ञान को भी। ये किरणें अंतःकरण के विभिन्न दर्पणों (A, B, C, D) तथा वस्तुगत जगत की दीवार पर पड़ रही हैं। यह स्वरूप-ज्ञान कहलाता है।
इसके अतिरिक्त, अंतःकरण के दर्पण (A', B', C', D') में परावर्तित प्रकाश भी पड़ता है, जिससे जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं में वस्तुओं का अनुभव संभव होता है। यह वृत्ति-ज्ञान कहलाता है।
सभी वृत्तियाँ केवल अंतःकरण से संबंधित होती हैं, जबकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव होता है। यह स्वरूप-ज्ञान जब वृत्तियों में प्रवेश करता है, तब अज्ञान का नाश कर देता है। केवल मन की वृत्तियाँ अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकतीं, जब तक कि उनमें स्वरूप-ज्ञान समाहित न हो। अतः आत्मा से उत्पन्न ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर सकता है, न कि केवल बुद्धि की वृत्तियाँ या असंख्य कर्म।
जिस प्रकार पुण्य कर्म पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वृत्ति-ज्ञान अज्ञान का नाश कर देता है। जैसे एक मणि अपने प्रकाश के कारण 'प्रकाशमान पत्थर' कहलाती है, वैसे ही वृत्ति-ज्ञान, जो अंतःकरण से उत्पन्न होता है, स्वयं को आत्मा से जुड़े होने के कारण ज्ञान कहा जाता है और इसे कर्म नहीं माना जाता।
संदेह: चूंकि स्वरूप-ज्ञान अज्ञान को गहन निद्रा में प्रकाशित करता है और दोनों उस अवस्था में सह-अस्तित्व रखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि वे प्रकाश और अंधकार की तरह एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। तो फिर यह स्वरूप-ज्ञान अज्ञान को कैसे नष्ट करता है?
स्पष्टीकरण:
स्वरूप-ज्ञान और अज्ञान स्वयं
विरोधी नहीं हैं,
किंतु जब स्वरूप-ज्ञान वृत्ति-ज्ञान के साथ संयुक्त
होता है, तब इनके बीच
विरोध उत्पन्न होता है।
संदेह: यदि वृत्ति-ज्ञान में प्रवेश करने वाला ज्ञान स्वयं स्वरूप-ज्ञान ही है, तो फिर अज्ञान के साथ विरोध क्यों उत्पन्न होता है?
स्पष्टीकरण:
जिस प्रकार सूर्य की किरणें
स्वयं में सूखी घास को
नहीं जलातीं, किंतु जब वे
किसी लेंस के माध्यम से
केंद्रित की जाती हैं, तो वे घास को
जला सकती हैं—
उसी प्रकार स्वरूप-ज्ञान,
जब यह वृत्ति-ज्ञान के माध्यम
से कार्य करता है, तभी अज्ञान का नाश
कर सकता है।
संदेह: यदि वृत्ति-ज्ञान के द्वारा अज्ञान और उसके परिणाम नष्ट हो जाते हैं, तो फिर अंत में केवल वृत्ति-ज्ञान और स्वरूप-ज्ञान ही शेष रहते हैं। ऐसी स्थिति में अद्वैतवाद की स्थापना कैसे संभव होगी?
स्पष्टीकरण:
जिस प्रकार मोरिंगा नट (सहजन का बीज)
गंदे पानी में डालने पर
उसे स्वच्छ कर देता है
और फिर स्वयं तलछट के
साथ मिलकर लुप्त हो जाता
है—
उसी प्रकार वृत्ति-ज्ञान,
अज्ञान और उसके प्रभावों को
नष्ट करके स्वयं भी विलीन
हो जाता है।
जब सभी वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, तब स्वरूप-ज्ञान का प्रतिबिंब भी अपने मूल स्रोत—आत्मा—में विलीन हो जाता है। उस अवस्था में केवल अद्वैत आत्मा ही शेष रह जाती है।
इस प्रकार, अज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकता है।
संदेह: क्या यह ज्ञान योग, पूजा, या अन्य क्रियाओं से प्राप्त किया जा सकता है?
स्पष्टीकरण:
नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा पर
निर्भर होता है
(वस्तुतंत्र), जबकि योग और पूजा
व्यक्ति के प्रयासों पर निर्भर होते हैं
(पुरुषतंत्र)।
● योग और पूजा मानसिक क्रियाएँ हैं, अतः वे केवल चित्त की एकाग्रता और अलौकिक शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं, परंतु ज्ञान नहीं।
● ज्ञान केवल आत्म-अनात्म विवेक (Atma-Anatma Vichara) से ही उत्पन्न होता है।
उदाहरण:
जिस प्रकार सोने,
बहुमूल्य रत्नों, या शालिग्राम (गंडकी नदी में मिलने
वाला पवित्र पत्थर)
की पहचान केवल उनके गुणों
की परीक्षा द्वारा संभव है—
न कि किसी तीर्थ-स्नान, कर्मकांड, या प्राणायाम द्वारा।
उसी प्रकार, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान केवल आत्म-अनात्म विवेक से ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि किसी अन्य साधन से।
जो भी इस आत्म-अनात्म विवेक का अभ्यास करता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर जीवन्मुक्त बन जाता है और अंततः विदेहमुक्ति प्राप्त करता है।
सभी वेदांत ग्रंथ एकमत होकर यही सत्य प्रतिपादित करते हैं।
जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को श्रद्धा और समर्पण के साथ सुनता और समझता है, वह शुद्ध, स्वतंत्र चेतना के रूप में प्रकाशित होता है।
वह कभी भी कर्तापन (agency) या भोग्यता (experiencership) का भ्रम नहीं करता, बल्कि स्वयं को शुद्ध साक्षी रूप आत्मा के रूप में देखता है।
वर्णक -7
आत्म-ज्ञान
इस अध्याय में आत्मा और अनात्मा के बीच भेद, उससे उत्पन्न आत्म-ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। अभी यह कहा गया कि आत्म-ज्ञान आत्मा और अनात्मा के बीच के भेद-विवेक से उत्पन्न होता है। आत्मा के बारे में स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है।
आत्मा या आत्मन तीन शरीरों से भिन्न है, तीन अवस्थाओं का साक्षी है, पंचकोशों से परे है और सत्-चित्-आनंद स्वरूप है। तीनों शरीर अनात्मा हैं। इनके लक्षण असत्यता, जड़ता और दुखमयता हैं। प्रत्येक शरीर के दो पक्ष होते हैं—एक समष्टि (सामूहिक) और दूसरा व्यष्टि (व्यक्तिगत)। यद्यपि इन विभाजनों को पहले अध्याय में ही विस्तृत रूप से समझाया गया है, फिर भी यहाँ उन्हें पुनः समझाने का प्रयोजन यह है कि विषय को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सके।
जैसे किसी वन को समष्टि (सामूहिक रूप) और किसी एक पेड़ को व्यष्टि (व्यक्तिगत रूप) कहा जा सकता है, वैसे ही किसी यौगिक वस्तु को समष्टि और उसके अवयवों को व्यष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार तीनों शरीरों के भी दो-दो पक्ष होते हैं—(i) समष्टि स्थूल शरीर, (ii) समष्टि सूक्ष्म शरीर, (iii) समष्टि कारण शरीर, (iv) व्यष्टि स्थूल शरीर, (v) व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और (vi) व्यष्टि कारण शरीर। इस प्रकार कुल छह रूप होते हैं।
आत्मा समष्टि और व्यष्टि दोनों से एक साथ सीमित प्रतीत होती है—समष्टि रूप में ईश्वर के रूप में और व्यष्टि रूप में जीव के रूप में। किंतु यह केवल प्रतीति मात्र है, वास्तविकता नहीं, क्योंकि आत्मा केवल एक ही है। माया के माध्यम से आत्मा स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रकट करती है और अविद्या के माध्यम से यह जीव रूप में प्रतीत होती है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जब तक कोई इन्हें वास्तविक मानता है, तब तक बंधन का नाश नहीं होता। शास्त्र, जो सभी जीवों के लिए माता के समान हैं, यह सिखाते हैं कि 'आत्मा स्वयं माया और अविद्या बनकर ईश्वर और जीव के रूप में प्रतीत होती है।'
ईश्वर समष्टि कारण शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रखता, क्योंकि अहंकार या 'मैं' की भावना, जो अभिमान का कारण होती है, वह महासुषुप्ति (महान गहरी निद्रा या प्रलय) में अव्यक्त स्थिति में रहती है। यह ईश्वर, जो समष्टि कारण शरीर का अधिपति है, अव्याकृत (अव्यक्त) और अंतर्यामी (अंतःनियंता) भी कहलाता है। इसे श्रेष्ठ प्रकार के भक्त जीव पूजनीय मानते हैं। जो लोग इस पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए शास्त्र इसे समष्टि सूक्ष्म शरीर से सीमित मानकर ध्यान करने की शिक्षा देते हैं। इस रूप में इसे हिरण्यगर्भ (स्वर्ण-अंडज से उत्पन्न), सूक्ष्मतम आत्मा (सभी प्रकट रूपों को अंदर से एक सूत्र में बाँधने वाला) और महा प्राण (संपूर्ण ब्रह्मांडीय जीवन-शक्ति) कहा जाता है।
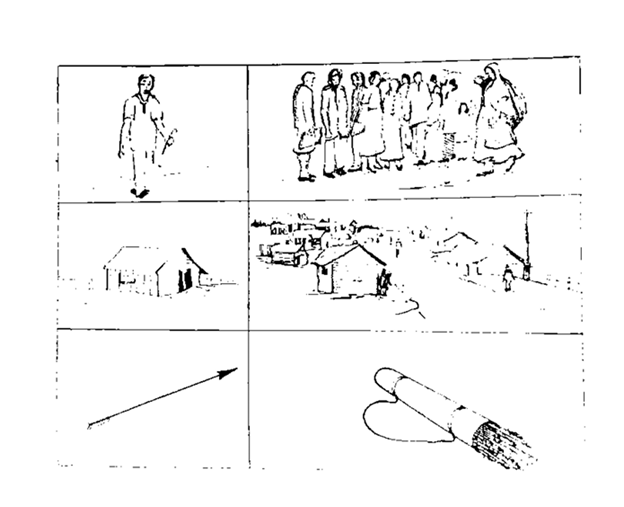 चित्र
7: व्यष्टि और समष्टि
चित्र
7: व्यष्टि और समष्टि
संशय: क्या हिरण्यगर्भ, जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, ईश्वर की भांति अपने शरीर से अभिमान नहीं करता?
स्पष्टीकरण: हाँ, हिरण्यगर्भ को भी समष्टि सूक्ष्म शरीर के प्रति अभिमान नहीं होता। यद्यपि अहंकार इस अवस्था में विद्यमान रहता है, फिर भी वह अपने को इस शरीर से जोड़कर नहीं देखता क्योंकि उसने अभी समष्टि स्थूल शरीर में प्रवेश नहीं किया है, जो अभिमान का केंद्र होता है। समष्टि सूक्ष्म शरीर केवल स्वप्न अवस्था की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति जाग्रत अवस्था में कार्य किए बिना स्वप्न में संस्कार नहीं ले सकता, वैसे ही बिना स्थूल शरीर के कोई अभिमान नहीं उत्पन्न होता।
जो लोग इस सूक्ष्म उपाधि के रूप में ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए शास्त्र समष्टि स्थूल शरीर में स्थित ईश्वर की उपासना का विधान करते हैं। इस अवस्था में ईश्वर को विराट, वैराज, या वैश्वानर कहा जाता है, जो अनगिनत रूपों में प्रकट होता है।
संशय: क्या इस विराट रूप में कोई अभिमान होता है?
स्पष्टीकरण: यदि विचार किया जाए, तो स्पष्ट होगा कि समष्टि स्थूल शरीर में भी ईश्वर को अभिमान नहीं होता क्योंकि इसका स्थूल शरीर समस्त जीवों के शरीरों का योगफल है। इसलिए इसमें व्यक्तिगत अहंकार की कोई संभावना नहीं होती।
जो लोग इन तीनों रूपों में भी ईश्वर का ध्यान करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए शास्त्र ब्रह्मा (सृष्टि करता), विष्णु (पालक) और रुद्र (संहारकर्ता) की उपासना की संस्तुति करते हैं। ये देवता भी उसी सर्वव्यापी ईश्वर के तीन गुणात्मक रूप हैं, जिन्हें रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण के अनुसार नाम दिए गए हैं। इन्हीं में से विष्णु अपने दैवीय अवतारों जैसे मत्स्य, कूर्म, आदि रूपों में अवतार लेकर दुष्टों का नाश और साधुओं की रक्षा करते हैं।
संशय: क्या इन अवतारों में अभिमान होता है?
स्पष्टीकरण: हाँ, इन अवतारों में अभिमान होता है। विशेष रूप से, ईश्वर इन रूपों में स्वयं को सीमित करता है ताकि वह अपने दायित्वों को निभा सके। यह अभिमान केवल कर्तव्य के लिए होता है, न कि अज्ञानवश। यह उसी प्रकार है जैसे कोई अभिनेता नाटक में किसी पात्र की भूमिका निभाने के लिए अस्थायी रूप से एक पहचान ग्रहण करता है।
संशय: यदि ईश्वर और जीव
दोनों ही अपने-अपने शरीरों के
साथ अभिमान करते हैं, तो उनमें क्या अंतर
है?
स्पष्टीकरण: ईश्वर का अभिमान केवल
अस्थायी और कृपा से प्रेरित
होता है, जबकि जीव का
अभिमान अज्ञानवश और स्थायी होता
है। जीव अपनी स्थूल और
सूक्ष्म उपाधियों के साथ "मैं"
और "मेरा"
का भाव रखता है, जबकि ईश्वर केवल संसार
की रक्षा हेतु अस्थायी रूप
से इस अभिमान को स्वीकार
करता है। इस प्रकार, ईश्वर और जीव में
स्पष्ट अंतर है।
जो लोग ईश्वर के इन व्यक्तिगत रूपों (साकार) का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मूर्तिपूजा का विधान किया गया है। कुछ लोग ईश्वर को मूर्तियों में पूजते हैं। किंतु यह समझना आवश्यक है कि ईश्वर की उपस्थिति मूर्ति के भीतर, अंतर्यामी रूप में होती है। केवल अज्ञानी लोग यह विवाद करते हैं कि विभिन्न देवताओं और मूर्तियों में भिन्न-भिन्न ईश्वर हैं। वास्तविकता यह है कि सभी देवताओं और उपास्य रूपों में एक ही सार्वभौम ईश्वर स्थित है।
संशय: यदि केवल एक ही ईश्वर सबमें समान रूप से विद्यमान है, तो फिर विभिन्न उपासनाओं और पूजा-पद्धतियों की आवश्यकता क्यों है?
स्पष्टीकरण: यह व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के हैं, ताकि उन्हें धीरे-धीरे अंतर्मुखी बनाया जा सके और अंततः उन्हें यह सिखाया जा सके कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही हैं। शास्त्र, प्रारंभिक अवस्था में भिन्न-भिन्न पूजाओं को स्वीकृति देते हैं ताकि जीव धीरे-धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सके।
अब यह
वर्णन किया जाएगा कि एक
परमात्मा किस प्रकार तीन व्यष्टि
शरीरों के माध्यम से जीवात्मा बनता है।
परमात्मा जब—
1. व्यष्टि कारण शरीर से संबद्ध होता है, तो उसे प्राज्ञ (Prajna) कहा जाता है।
○ इसे "परमार्थिक" या "अविद्या से सीमित चेतना" भी कहा जाता है।
2. व्यष्टि सूक्ष्म शरीर से संबद्ध होने पर, इसे तैजस (Taijasa) कहते हैं।
○ इसे "स्वप्न-कल्पित आत्मा" या "प्रतिभासिक आत्मा" भी कहा जाता है।
3. व्यष्टि स्थूल शरीर से संबद्ध होने पर, इसे विश्व (Visva) कहा जाता है।
○ इसे "व्यवहारिक आत्मा" या "चिदाभास" (परमात्मा का प्रतिबिंब) भी कहते हैं।
संशय: जीव को इन तीन शरीरों की आवश्यकता क्यों होती है?
स्पष्टीकरण: जीव आत्मा, परमात्मा का ही प्रतिबिंब (Reflection) है, जो अंतःकरण (Antahkarana) में प्रतिबिंबित होता है।
● अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में स्थित होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर का होना आवश्यक है।
● बिना स्थूल शरीर के कर्म और कर्तृत्व की अभिव्यक्ति संभव नहीं, इसलिए स्थूल शरीर की भी आवश्यकता होती है।
● इन दोनों शरीरों का कारण कारण शरीर है, इसलिए कारण शरीर का होना भी अनिवार्य है।
● इस प्रकार, तीनों शरीरों की आवश्यकता निर्विवाद है।
संशय: क्या जीव को अपने तीन शरीरों के साथ अभिमान होता है?
स्पष्टीकरण: हाँ, यदि जीव के इन शरीरों से अभिमान न हो तो उसमें कर्तृत्व की भावना नहीं आ सकती।
● यदि कर्तृत्व नहीं होगा, तो कर्म भी नहीं होगा।
● यदि कर्म नहीं होगा, तो शरीर भी प्राप्त नहीं होगा।
● यदि शरीर नहीं होगा, तो जीव की सत्ता ही नहीं रह सकेगी।
इसलिए, अभिमान ही जीव के अस्तित्व का कारण है।
संशय: क्या कोई उदाहरण है जिससे यह सिद्ध हो सके?
स्पष्टीकरण:
1. देवदत्त नामक व्यक्ति अपने पुत्र के लिए पिता है और अपने पौत्र के लिए दादा।
○ वह एक ही व्यक्ति होते हुए भी, अलग-अलग संबंधों के कारण भिन्न-भिन्न रूप धारण करता है।
○ इसी प्रकार, परमात्मा माया और अविद्या की उपाधियों से ईश्वर और जीव के रूप में प्रतीत होता है।
संशय: इस उदाहरण से केवल
नाम का भेद सिद्ध होता
है, किंतु ईश्वर सर्वज्ञ और
जीव अल्पज्ञ क्यों होता है?
स्पष्टीकरण:
1. झील
और घड़े के पानी का
उदाहरण
○ झील का जल संपूर्ण गाँव की प्यास बुझाने में सक्षम है, जबकि घड़े का जल केवल एक परिवार की प्यास बुझा सकता है।
○ इसी प्रकार, ईश्वर की ज्ञान शक्ति असीमित है, जबकि जीव की शक्ति सीमित है।
2. दीपक
और मशाल का उदाहरण
○ मशाल का प्रकाश संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर सकता है, जबकि दीपक का प्रकाश केवल एक कमरे तक सीमित होता है।
○ इसी प्रकार, ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ।
इन सभी भेदों का कारण माया और अविद्या की उपाधियाँ (limiting adjuncts) हैं, न कि आत्मा का कोई भेद।
अतः वेदांत का निष्कर्ष यही है कि ईश्वर और जीव का स्वरूप मूलतः एक ही है।
जिसे माया और अविद्या की उपाधियाँ सीमित करती हैं, शब्दों के प्रत्यक्ष अर्थ से बंधा हुआ है। इसलिए, महावाक्य "तत् त्वम् असि" (That Thou Art) के शब्दों "तत्" (That) और "त्वम्" (Thou) के लक्ष्यार्थ (Indicative Meaning) को ग्रहण करना आवश्यक है।
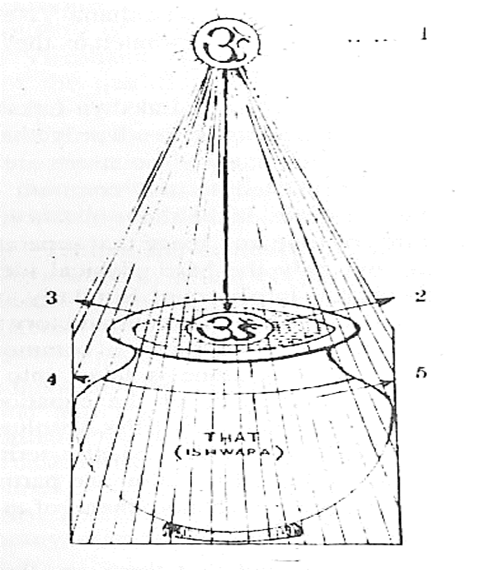
चित्र 8: "तत्" (Tat) की स्थिति
"तत्" (Tat) की स्थिति
1. ब्रह्म (Brahman) – शुद्ध चैतन्य, निर्गुण और निराकार।
2. माया (Maya) – ब्रह्म की शक्ति, जो ब्रह्म को ईश्वर रूप में प्रतिबिंबित करती है।
3. ईश्वर का प्रतिबिंबित चैतन्य (Reflected Consciousness of Brahman, i.e., Isvara) – ब्रह्म का माया में प्रतिबिंब।
4. ईश्वर की उपाधि (Upadhi or Limiting Adjunct of Isvara) – वह माध्यम (माया) जिसके द्वारा ब्रह्म, ईश्वर के रूप में प्रकट होता है।
5. ब्रह्म का अनुपहित शुद्ध चैतन्य (Unassociated Pure Consciousness of Brahman) – जो किसी भी उपाधि से सीमित नहीं है।
लक्षणा वृत्ति के तीन प्रकार (Three Types of Lakshana-Vritti)
1. जहल्लक्षणा (Jahallakshana) – पूरी तरह से शब्द के प्रत्यक्ष अर्थ का त्याग करना।
2. अजहल्लक्षणा (Ajahallakshana) – प्रत्यक्ष अर्थ को बनाए रखना, लेकिन उसका विस्तार करना।
3. जहदजहल्लक्षणा (Jahadajahallakshana) – कुछ भाग का त्याग और कुछ भाग का ग्रहण करना (भगत्याग-लक्षणा)।
उदाहरण
1. जहल्लक्षणा
(Jahallakshana) – "गंगायां घोषः"
(Gangayam Ghoshah)
○ प्रत्यक्ष अर्थ: "ग्वालों का गाँव गंगा के ऊपर स्थित है" (जो असंभव है)।
○ लक्षणा अर्थ: "ग्वालों का गाँव गंगा के किनारे है" (शब्द 'गंगा' का प्रत्यक्ष अर्थ छोड़कर नया अर्थ ग्रहण किया गया)।
2. अजहल्लक्षणा
(Ajahallakshana) – "सोनो धावति"
(Sono Dhavati)
○ प्रत्यक्ष अर्थ: "लाल दौड़ रहा है" (लाल रंग कैसे दौड़ सकता है?)
○ लक्षणा अर्थ: "लाल घोड़ा दौड़ रहा है" (शब्द 'लाल' को बनाए रखते हुए उसके अर्थ को विस्तृत किया गया)।
3. जहदजहल्लक्षणा
(Jahadajahallakshana) – "सोऽयम् देवदत्तः"
(Soyam Devadattah)
○ प्रत्यक्ष अर्थ: "यह वही देवदत्त है", लेकिन यह कहने में समय और स्थान अलग हो सकते हैं।
○ लक्षणा अर्थ: "समय और स्थान का त्याग कर, केवल देवदत्त के अस्तित्व को स्वीकार करना"।
महावाक्य "तत् त्वम् असि" (That Thou Art) की व्याख्या
यदि हम केवल शब्दों के प्रत्यक्ष अर्थ को लें, तो यह समानता असंभव होगी, क्योंकि:
● "तत्" (That) शब्द का प्रत्यक्ष अर्थ है ईश्वर (जो माया से प्रतिबिंबित है)।
● "त्वम्" (Thou) शब्द का प्रत्यक्ष अर्थ है जीव (जो अविद्या से प्रतिबिंबित है)।
● "असि" (Art) शब्द कहता है कि दोनों एक हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अर्थ विरोधाभासी हैं।
इसलिए, यहाँ जहदजहल्लक्षणा (Jahadajahallakshana) लागू होती है।
● हम माया और अविद्या (जो दोनों विभाजन का कारण हैं) को त्याग देते हैं।
● हम केवल ब्रह्म (शुद्ध चैतन्य) को स्वीकार करते हैं, जो दोनों में समान है।
इस प्रकार, "तत् त्वम् असि" का लक्ष्यार्थ (Indicative Meaning) यह है कि ईश्वर और जीव वस्तुतः एक ही शुद्ध चैतन्य हैं।
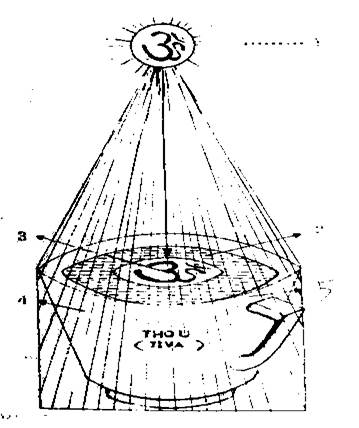
चित्र 9: "त्वम्" (Tvam) की स्थिति
"त्वम्" (Tvam) की स्थिति
1. ब्रह्म (Brahman) – शुद्ध चैतन्य, जो नित्य और निरपेक्ष है।
2. अविद्या (Avidya) – अज्ञान, जो आत्मा पर उपाधि के रूप में प्रतिबिंबित होती है।
3. ब्रह्म का प्रतिबिंबित चैतन्य (Reflected Consciousness of Brahman, i.e., Chidabhasa) – आत्मा का प्रतिबिंब, जो सीमित रूप में जीव के रूप में प्रकट होता है।
4. जीव की उपाधि (Upadhi or Limiting Adjunct of Jiva) – वह माध्यम (अविद्या), जिससे ब्रह्म जीव रूप में प्रकट होता है।
5. निर्लिप्त शुद्ध चैतन्य जिसे कूटस्थ कहा जाता है (Unassociated Pure Consciousness called Kutastha) – आत्मा का शुद्ध रूप, जो किसी भी उपाधि से सीमित नहीं है।
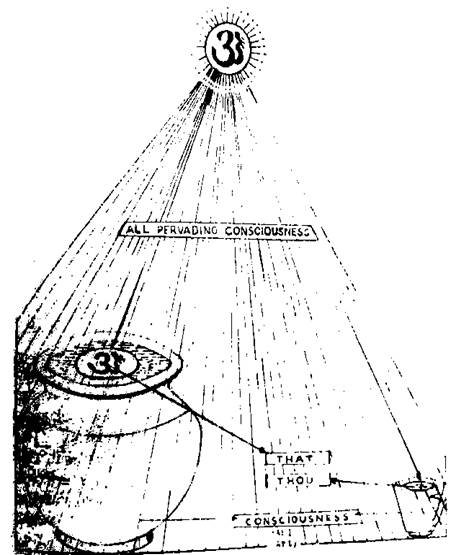
चित्र10: "असि" (Asi) की स्थिति – महावाक्य "तत् त्वम् असि" में
"असि" (Asi) की स्थिति – महावाक्य "तत् त्वम् असि" में
● "तत्" (That) – ईश्वर का शुद्ध चैतन्य (Brahma-Chaitanya in Isvara)
● "त्वम्" (Thou) – जीव का शुद्ध चैतन्य (Kutastha-Chaitanya in Jiva)
● "असि" (Art) – इन दोनों के बीच समानता या एकत्व (Oneness)
महावाक्य "तत् त्वम् असि" यह सिखाता है कि "तत्" (That) और "त्वम्" (Thou) के विरोधाभासी भागों को त्यागकर केवल समान चैतन्य (Unassociated Pure Consciousness) को स्वीकार किया जाए।
महावाक्य "तत् त्वम् असि" का वास्तविक अर्थ
1. उदाहरण:
○ जिस प्रकार देवदत्त अपने "पिता" और "दादा" जैसे विशेषणों को त्यागकर केवल स्वयं रहता है।
○ जिस प्रकार झील और घड़े के भेद को हटाने पर केवल पानी बचता है।
○ जिस प्रकार बड़े और छोटे दीपकों के भेद को छोड़ने पर केवल प्रकाश शेष रहता है।
○ उसी प्रकार माया और अविद्या को त्यागने पर केवल अद्वैत आत्मा (Sat-Chit-Ananda) शेष रहता है।
2. महत्वपूर्ण निष्कर्ष:
○ महावाक्य "तत् त्वम् असि" का वास्तविक अर्थ ब्रह्म-चैतन्य (Brahman Consciousness) और कूटस्थ-चैतन्य (Kutastha Consciousness) की एकता है।
○ उपाधियों (माया और अविद्या) को त्यागकर जीव और ईश्वर की भिन्नता समाप्त हो जाती है।
○ जो व्यक्ति इस सत्य का अनुभव करता है, वही "अहं ब्रह्मास्मि" (Aham Brahmasmi) या "ब्रह्मैवाहमस्मि" (Brahmaiva Aham Asmi) का साक्षात अनुभव करता है।
जो साधक इस महावाक्य के वास्तविक अर्थ को समझकर यह अनुभव करता है कि "मैं ही परमात्मा हूँ", वह वास्तव में जीवन्मुक्त (Jivanmukta) और सिद्ध आत्मा (Perfected Soul) होता है। समस्त वेदांत ग्रंथ इसी सत्य को उद्घोषित करते हैं।
वर्णक 8
आत्मा तीनों शरीरों से भिन्न है
अगले चार अध्यायों में, जो इस अध्याय से शुरू होते हैं, परमात्मा या परम आत्मा को चार विभिन्न तरीकों से समझाया गया है—(1) शरीरत्रय-विलक्षण या तीन शरीरों से पृथक, (2) अवस्थात्रय-साक्षी या तीन अवस्थाओं का साक्षी, (3) पंचकोश-व्यतिरीक्त या पंचकोशों से परे और (4) सत्-चित्-आनंद स्वरूप या शुद्ध अस्तित्व-चेतना-आनंद। इन चारों विवरणों में, शरीरत्रय-विलक्षणत्व (तीन शरीरों से पृथकता) और पंचकोश-व्यतिरीक्तत्व (पंचकोशों से परे होना) को तकनीकी रूप से "अतद्व्यावृत्ति-लक्षण" कहा जाता है, अर्थात् "जो नहीं है, उसका निषेध करके वर्णन करना"। अवस्थात्रय-साक्षित्व (तीन अवस्थाओं का साक्षी होना) को "तातस्थ-लक्षण" कहा जाता है, अर्थात् बाह्य विशेषताओं द्वारा वर्णन। सत्-चित्-आनंद स्वरूपत्व (अस्तित्व-चेतना-आनंद स्वरूप) को "स्वरूप-लक्षण" कहा जाता है, अर्थात् मूलभूत स्वरूप द्वारा वर्णन। इन तीनों लक्षणों को आगे विस्तार से समझाया गया है।
आत्मा का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करते हुए उसे "नेति-नेति" (यह नहीं, यह भी नहीं) के माध्यम से आकाश से लेकर तीन शरीरों तक सभी दृश्य चीज़ों का निषेध करके समझाना "अतद्व्यावृत्ति-लक्षण" कहलाता है। आत्मा को संपूर्ण ब्रह्मांड के आधारभूत तत्व के रूप में प्रस्तुत करना "तातस्थ-लक्षण" कहलाता है, और इसे नित्य, पूर्ण, अस्तित्व-चेतना-आनंद स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करना "स्वरूप-लक्षण" कहलाता है।
इस आठवें अध्याय में शरीरत्रय-विलक्षण को समझाया गया है। जब तक तीन शरीरों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तब तक उनसे भिन्न आत्मा का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। इसलिए तीन शरीरों का विस्तृत विवरण देना आवश्यक है। ये तीन शरीर हैं—(1) स्थूल शरीर या भौतिक शरीर, (2) सूक्ष्म शरीर और (3) कारण शरीर।
स्थूल शरीर वह भौतिक शरीर है जिसे सभी देख सकते हैं और जिसमें हाथ, पैर आदि विभिन्न अंग होते हैं। यह एक कठोर स्तंभ की भाँति प्रतीत होता है। सूक्ष्म शरीर सत्रह अवयवों से बना होता है। कारण शरीर या कारणात्मक शरीर वास्तव में अज्ञान या अविद्या है। इन शरीरों को "नष्ट होने वाले" कहा जाता है। "शरीर" शब्द "शृ" धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है "क्षय होना"। क्योंकि भोजन के अभाव में भौतिक शरीर क्षीण हो जाता है; बल्कि भोजन मिलने पर भी यह किसी रोग के कारण क्षीण हो सकता है; और रोग के अभाव में भी यह केवल वृद्धावस्था की प्रक्रिया के कारण क्षीण हो जाता है।
सूक्ष्म शरीर भी कुछ समय के लिए जीवित रहता है और फिर एक कली की तरह नष्ट हो जाता है। यह प्रेम, घृणा आदि मानसिक प्रवृत्तियों के विकास से पुष्पित होता है और इनके अभाव में क्षीण हो जाता है। कारण शरीर भी "मैं जीव हूँ" इस भावना से पुष्ट होता है और "अहं ब्रह्मास्मि" (मैं ब्रह्म हूँ) इस विचार से नष्ट हो जाता है।
इस प्रकार, अज्ञानी व्यक्तियों में सूक्ष्म और कारण शरीरों का विकास देखा जाता है, जबकि ज्ञानी व्यक्तियों में इनका क्षय होता है। इसलिए वृद्धावस्था किसी न किसी रूप में तीनों शरीरों को प्रभावित करती है। इस कारण इन्हें "शरीर" या "नष्ट होने वाला" कहा जाता है। शरीर को "देह" भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है "जो जलाया जाता है"। इसकी व्युत्पत्ति "दह्यते इति देहः" से हुई है, जहाँ "दह" धातु का अर्थ "जलाना" होता है।
संदेह: स्थूल शरीर को तो अग्नि द्वारा जलाया जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर को जलते हुए कोई नहीं देखता, फिर इन्हें "देह" क्यों कहा जाता है?
स्पष्टीकरण: तीनों शरीर "तापत्रय" (तीन प्रकार के कष्ट) से जलते हैं:
1. आध्यात्मिक (Adhyatmika) - शरीर और मन के आंतरिक कष्ट,
2. आधिदैविक (Adhidaivika) - देवताओं, ग्रहों, ऋतुचक्र आदि से उत्पन्न कष्ट,
3. आधिभौतिक (Adhibhautika) - अन्य जीवों से उत्पन्न कष्ट।
स्थूल शरीर पंचमहाभूतों से बना है, इसलिए यह स्थूल प्रतीत होता है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना है और इसमें ठोसपन नहीं होता, इसलिए यह सूक्ष्म कहलाता है।
सूक्ष्म शरीर को "लिंग शरीर" भी कहा जाता है। ‘लिंग’ शब्द का अर्थ है "जो स्वयं अदृश्य रहकर भी अन्य वस्तुओं को प्रकट करता है"। कारण शरीर को कारण इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य दो शरीरों का मूल कारण है।
संदेह: पहले कहा गया था कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर पंचमहाभूतों से बने हैं, अब कहा जा रहा है कि वे कारण शरीर से उत्पन्न होते हैं। यह विरोधाभास क्यों?
स्पष्टीकरण: सृष्टि के दो प्रकार हैं:
1. क्रम सृष्टि (Krama Srishti) - जिसमें मूल प्रकृति से पंचमहाभूतों का विकास क्रमशः होता है।
2. युगपत् सृष्टि (Yugapat Srishti) - जिसमें अज्ञान के कारण समस्त जगत एक साथ उत्पन्न प्रतीत होता है।
पहले वर्णन क्रम सृष्टि के अनुसार था और अब वर्णन युगपत् सृष्टि के अनुसार है, इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है।
संदेह: स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कैसे जाना जाए?
स्पष्टीकरण: यद्यपि सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष नहीं दिखता, फिर भी इसकी उपस्थिति इसके सत्रह अवयवों के कार्यों से जानी जा सकती है।
संदेह: क्या स्थूल और सूक्ष्म शरीर मिलकर इन कार्यों को संपन्न नहीं कर सकते?
स्पष्टीकरण: कोई भी क्रिया केवल स्थूल शरीर द्वारा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, अग्नि जलाने का कार्य तभी कर सकती है, जब वह ईंधन के सहारे प्रकट हो, लेकिन जलाने की शक्ति अग्नि की ही होती है, ईंधन की नहीं। उसी प्रकार, देखने, सुनने आदि की क्रिया सूक्ष्म शरीर के कारण होती है, न कि स्थूल शरीर के कारण।
सूक्ष्म शरीर के सत्रह अवयव:
1. पाँच
ज्ञानेन्द्रियाँ (इन्द्रियाँ):
○ श्रोत्र (कर्ण) - सुनना (दिशा देवता द्वारा प्रेरित),
○ त्वचा - स्पर्श अनुभव करना (वायु देवता द्वारा प्रेरित),
○ चक्षु (नेत्र) - रंग एवं आकार देखना (सूर्य देवता द्वारा प्रेरित),
○ जिह्वा (रसना) - स्वाद अनुभव करना (वरुण देवता द्वारा प्रेरित),
○ घ्राण (नाक) - गंध अनुभव करना (अश्विनी कुमार द्वारा प्रेरित)।
2. पाँच
कर्मेन्द्रियाँ (क्रियाएँ करने वाले अंग):
○ वाक् (जिह्वा) - बोलने की शक्ति (अग्नि देवता द्वारा प्रेरित),
○ पाणि (हाथ) - ग्रहण करना (इन्द्र देवता द्वारा प्रेरित),
○ पाद (पैर) - चलना (उपेन्द्र द्वारा प्रेरित),
○ पायु (गुदा) - मल त्याग (मृत्यु देवता द्वारा प्रेरित),
○ उपस्थ (गुप्तेंद्रिय) - संतति एवं सुख (प्रजापति द्वारा प्रेरित)।
3. पाँच
प्राण (जीवनशक्ति के प्रकार):
○ प्राण - श्वसन (हृदय में स्थित),
○ अपान - मल-मूत्र त्याग (गुदा में स्थित),
○ व्यान - शरीर में रक्तसंचार (संपूर्ण शरीर में व्याप्त),
○ उदान - चेतना जागृत करना (कंठ में स्थित),
○ समान - पाचन क्रिया (नाभि में स्थित)।
4. मन
और बुद्धि:
○ मन (सोचने, संकल्प-विकल्प करने वाला),
○ बुद्धि (निर्णय करने वाला)।
निष्कर्ष:
स्थूल शरीर प्रत्यक्ष है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को इसके कार्यों से जाना जाता है। कारण शरीर अज्ञानस्वरूप है। इन तीनों शरीरों से जो परे है, वही परमात्मा है।
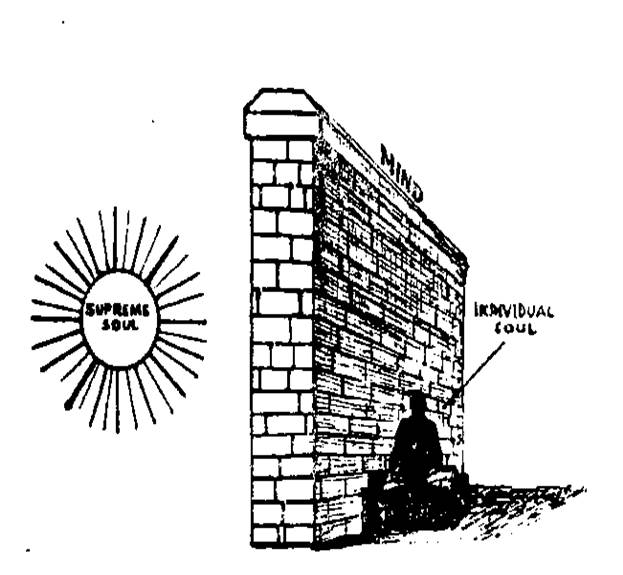
चित्र 11: मन क्या है?
मन क्या है?
"जो तुम्हें भगवान से अलग करता है, वही मन है। जो दीवार तुम्हारे और भगवान के बीच खड़ी है, वह मन है। मन कुछ और नहीं बल्कि संस्कारों, इच्छाओं, भावनाओं और विचारों का संग्रह है। यह केवल आदतों का एक समूह मात्र है।"
—स्वामी
शिवानंद
अंतःकरण (मन) के चार अंग
अंतःकरण चार भागों में विभाजित है:
1. मन (Manas) – विचार और संकल्प-विकल्प करता है। (देवता: चंद्र)
2. बुद्धि (Buddhi) – निर्णय करने की शक्ति। (देवता: ब्रह्मा)
3. अहंकार (Ahamkara) – 'मैं' की भावना और आसक्ति। (देवता: रुद्र)
4. चित्त (Chitta) – स्मरण शक्ति। (देवता: विष्णु)
कुछ ग्रंथों में सूक्ष्म शरीर को 16 तत्वों वाला माना जाता है, जहां अंतःकरण को एक ही तत्व माना गया है। अन्य ग्रंथों में इसे 17 तत्वों का बताया गया है, जिसमें अंतःकरण को मन और बुद्धि के रूप में गिना गया है। कहीं-कहीं इसे 19 तत्वों का भी कहा गया है, जिसमें अंतःकरण को चार भागों—मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—में विभाजित किया गया है।
क्या कारण शरीर भी नष्ट होता है?
कारण शरीर (अज्ञान) को दोनों शरीरों (स्थूल और सूक्ष्म) का कारण कहा जाता है। यह जीव और ईश्वर दोनों के लिए पहला शरीर माना जाता है। अतः यह अन्य दो शरीरों का कारण बनता है।
संदेह: क्या कोई प्रमाण है कि अज्ञान ही कारण शरीर है?
स्पष्टीकरण: हाँ, इसके तीन प्रमाण हैं:
1. श्रुति (शास्त्र प्रमाण) – वेदों में अज्ञान को कारण कहा गया है।
2. युक्ति (तर्क प्रमाण) – प्रत्येक प्रभाव का कोई न कोई कारण होता है।
3. अनुभव (प्रत्यक्ष प्रमाण) – जब कोई कहता है, "मैं अज्ञानी हूँ," तो अज्ञान का अनुभव होता है।
आत्मा का स्वरूप
ब्रह्म को "सर्वव्यापक" कहा गया है, क्योंकि वह अविभाज्य रूप से सर्वत्र व्याप्त है। सभी उपनिषदें इस परम सत्य की घोषणा करती हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है।
आत्मा का स्वरूप सत्-चित्-आनंद (अस्तित्व-चेतना-आनंद) है।
● सत् (अस्तित्व) – जो कभी नष्ट नहीं होता।
● चित् (चेतना) – जो स्वयं प्रकाशित है।
● आनंद (सुख) – जो स्वयं में परिपूर्ण है।
इसके विपरीत, अनात्मा (शरीर, मन आदि) की प्रकृति है:
● अनृत (असत्य) – जो समय के साथ बदलता रहता है।
● जड़ता (अचेतनता) – जिसमें स्वयं से प्रकाश नहीं होता।
● दुःख (कष्ट) – जो परिवर्तनशील और सीमित है।
संदेह: आत्मा और अनात्मा में भेद कैसे करें?
स्पष्टीकरण: जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के भौतिक लक्षण भिन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्मा (सत्-चित्-आनंद) और अनात्मा (अनृत-जड़-दुःख) में मूल अंतर है।
सत् और असत् का अंतर:
● जो तीनों कालों (भूत, वर्तमान, भविष्य) में बना रहता है, वह सत् है।
● जो कभी था ही नहीं, लेकिन भ्रमवश प्रतीत होता है, वह असत् है।
उदाहरण:
● रात्रि में रस्सी को सांप समझने का भ्रम होता है।
● यह सांप तीनों कालों में कभी भी वास्तविक नहीं था।
● रस्सी ही सदा वास्तविक थी।
इसी प्रकार शरीर, मन, बुद्धि आदि असत् हैं, जबकि आत्मा सत् है।
चित् और जड़ का अंतर:
● चित् (चेतना) स्वयं प्रकाशित होती है और अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करती है।
● जड़ (अचेतन) न स्वयं को प्रकाशित कर सकता है, न अन्य वस्तुओं को।
उदाहरण:
● सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाश देता है।
● मिट्टी का घड़ा स्वयं प्रकाशित नहीं होता।
इसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है, जबकि शरीर और मन अचेतन हैं।
आनंद और दुःख का अंतर:
● आनंद पूर्ण और स्वतंत्र होता है।
● दुःख तीन प्रकार के होते हैं:
1. आध्यात्मिक (Adhyatmika) – शरीर और मन के कष्ट।
2. आधिभौतिक (Adhibhautika) – अन्य प्राणियों से उत्पन्न कष्ट।
3. आधिदैविक (Adhidaivika) – प्राकृतिक आपदाएँ।
उदाहरण:
● अमृत का स्वभाव सुखदायक होता है।
● विष का स्वभाव घातक होता है।
इसी प्रकार आत्मा आनंदमय है, जबकि संसार दुःखमय है।
संदेह: इस विवेचना का क्या लाभ है?
स्पष्टीकरण: जो आत्मा को जान लेता है, वह शरीर और मन के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता।
उदाहरण:
● सूर्य बर्तन में रखे जल को प्रकाशित करता है, लेकिन जल की स्थिति (शुद्ध या अशुद्ध) से प्रभावित नहीं होता।
● आत्मा शरीर और मन के सभी विकारों को प्रकाशित करता है, लेकिन स्वयं अछूता रहता है।
निष्कर्ष
यह सिद्ध हो गया कि आत्मा:
1. सत् है – जैसे रस्सी सदा रहती है, वैसे ही आत्मा नित्य है।
2. चित् है – जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, वैसे ही आत्मा स्वप्रकाश है।
3. आनंद है – जैसे अमृत सुखदायक है, वैसे ही आत्मा आनंदस्वरूप है।
जो इस ज्ञान को गुरु से प्राप्त करता है और स्वयं अनुभव करता है, वही सच्चा मुक्त पुरुष है। यही वेदांत का अंतिम निष्कर्ष है।
वर्णक 9
आत्मा तीनों अवस्थाओं का साक्षी है
स्वयं को इंगित करने के चार तरीकों में से, अर्थात्, (i) शरीरत्रय-विलक्षण या तीन शरीरों से भिन्न, (ii) अवस्थात्रय-साक्षी या तीन अवस्थाओं का साक्षी, (iii) पंचकोश-व्यतिरेक या पाँच कोशों से परे, और (iv) सत्-चित्-आनंद-स्वरूप या अस्तित्व-चेतना-आनंद-परम, केवल पहले पक्ष का वर्णन आठवें अध्याय में किया गया था। अब इस अध्याय में इसकी तीन अवस्थाओं की साक्षी रूपी प्रकृति को समझाया जा रहा है।
मन का स्वभाव सात्त्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का होता है, लेकिन इसमें सात्त्विक गुण प्रधान होता है। आत्मा को केवल सात्त्विक मन के माध्यम से ही जाना जा सकता है, न कि राजसिक या तामसिक मन के द्वारा। सात्त्विक गुण सूक्ष्म होता है, राजस गतिशील होता है और तमस स्थूल होता है। इसलिए, जैसे एक बड़ी लकड़ी का बीम एक छोटे छिद्र से नहीं गुजर सकता, जिसमें केवल धुआँ ही प्रवेश कर सकता है, और जैसे एक टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में सूक्ष्म रंगों को भली-भांति पहचाना नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मा, जो अत्यंत सूक्ष्म है, तामसिक या राजसिक मन के द्वारा नहीं जानी जा सकती। इसे केवल सात्त्विक मन से ही अनुभूत किया जा सकता है। इसलिए, इसे एकाग्रता द्वारा सही तरीके से समझना चाहिए।
अब तीन अवस्थाओं की प्रकृति को समझाया गया है। ये तीन अवस्थाएँ हैं: (i) जाग्रत (जाग्रत अवस्था), (ii) स्वप्न (स्वप्न अवस्था) और (iii) सुषुप्ति (गहरी निद्रा अवस्था)। इंद्रियों द्वारा बाहरी वस्तुओं का अनुभव जाग्रत अवस्था को इंगित करता है। जब मन अपनी जाग्रत अवस्था में अर्जित छापों की सहायता से भोक्ता और भोग्य रूपों में रूपांतरित होता है, तो इसे स्वप्न अवस्था कहा जाता है।
"यह संसार एक दर्पण में दिखने वाले नगर की भाँति है। माया की शक्ति के कारण यह बाहर विद्यमान प्रतीत होता है, जैसे स्वप्न की अवस्था में अनुभव किया गया संसार वास्तव में जीव के मन के भीतर ही स्थित होता है।"
-डाक्षिणामूर्ति स्तोत्र, भगवान शंकराचार्य
अज्ञान की वह अवस्था, जो केवल निष्कलंक साक्षी द्वारा जानी जाती है और जो जाग्रत तथा स्वप्न अवस्थाओं के विलय के बाद कारण अज्ञान में परिवर्तित हो जाती है, सुषुप्ति अवस्था कहलाती है।
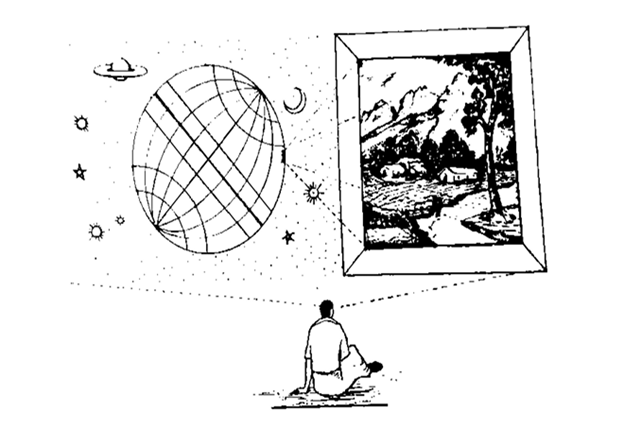
चित्र 12. अनुभूति का ब्रह्मांड.
संदेह: आत्मा तीन अवस्थाओं का साक्षी कैसे बनता है?
स्पष्टीकरण: सर्वप्रथम, साक्षी-स्वरूपता आत्मा की स्वाभाविक विशेषता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है: जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति और उसकी क्रियाओं को देखता है, परंतु स्वयं किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, तो उसे उस व्यक्ति का साक्षी कहा जाता है। इसी प्रकार, एक संन्यासी जो आगंतुक को देखता है, उसकी स्थिति और कार्यों को देखता है, परंतु स्वयं अप्रभावित रहता है, वह उस आगंतुक का साक्षी कहलाता है। उसी प्रकार, आत्मा विभिन्न जीवों, उनके अस्तित्व की अवस्थाओं और उनके कार्यों को देखती है, फिर भी स्वयं अपरिवर्तित बनी रहती है।
अब तीन अवस्थाओं को एक उदाहरण से समझाया गया है। जाग्रत अवस्था को एक बड़े नगर के समान माना जा सकता है। स्वप्न अवस्था एक महल के प्रांगण की तरह है और सुषुप्ति अवस्था महल के आंतरिक कक्ष की तरह है। जीवात्मा, जो क्रमशः इन तीन अवस्थाओं से जुड़ती है, राजा के समान है, जो महल का स्वामी है। वह नगर में जाता है, वहाँ उसे इच्छाओं और द्वेष की वस्तुएँ मिलती हैं और वह सुख-दुःख का अनुभव करता है। महल में लौटने पर वह सीमित रूप से सुख-दुःख का अनुभव करता है। परंतु जब वह आंतरिक कक्ष में प्रवेश करता है, तो सभी क्रियाएँ छोड़कर वह अपनी प्रिय संगिनी के साथ मौन आनंद का अनुभव करता है। इसी प्रकार, जाग्रत अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल शरीर के साथ कार्य करता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर से अनुभव करता है और सुषुप्ति में कारण शरीर में लीन होकर आनंद का अनुभव करता है।
कूटस्थ आत्मा तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप में बनी रहती है और आकाश की तरह असंग होती है। इस साक्षी-चेतना-स्वरूप आत्मा को शास्त्र, तर्क और अनुभव से समझना चाहिए।
शास्त्रों में कहा गया है कि 'यह साक्षी, चेतना, निरपेक्ष और निर्गुण है।' ऊपर दिया गया नगर का उदाहरण युक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तीनों अवस्थाओं के अस्तित्व का अनुभव-आधारित प्रमाण इस प्रकार है: प्रतिदिन हम बीते हुए दिन की तीन अवस्थाओं को याद करते हैं। यह एक मानसिक नियम है कि बिना पूर्व अनुभव के स्मरण संभव नहीं है। इसलिए, यह निश्चित है कि हम प्रतिदिन इन तीन अवस्थाओं का अनुभव करते हैं।
चूँकि जीव अतीत और भविष्य में तीनों अवस्थाओं का अनुभव करता है, और आत्मा सदैव एक अपरिवर्तनीय साक्षी के रूप में बनी रहती है, इस प्रकार आत्मा की शाश्वतता अनुभव के माध्यम से सिद्ध होती है।
संशय: इस संसार में सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जो भी अपनी अवस्थाओं का साक्षी होता है, वही उनका अनुभवकर्ता भी होता है। यदि ऐसा है, तो तीन अवस्थाओं का साक्षी उनके अनुभवकर्ता से बिल्कुल भिन्न कैसे हो सकता है?
स्पष्टीकरण: इन अवस्थाओं का अनुभव करने वाला, जिसे चिदाभास कहा जाता है, केवल अंतःकरण (अंतःकरण या आंतरिक उपकरण) में प्रतिबिंबित चेतना है। यह काल्पनिक और अवास्तविक है। इसे ही जीव कहा जाता है।
गहरी निद्रा की अवस्था में, जब अंतःकरण लय को प्राप्त हो जाता है, तो जीव भी लुप्त हो जाता है। तब वह उस अवस्था का साक्षी कैसे हो सकता है? चूँकि शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि तीनों अवस्थाओं का एकमात्र साक्षी आत्मा ही है, जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित होती है, इसलिए आत्मा को ही गहरी निद्रा की अवस्था का साक्षी माना जाना चाहिए। साथ ही, यह स्पष्ट है कि आत्मा जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं की भी साक्षी है।
चूँकि जीव परिवर्तनशील है, इसलिए उसे साक्षी नहीं कहा जा सकता, जबकि 'साक्षी' शब्द आत्मा के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनीय होती है। यह तथ्य कि जीव परिवर्तनशील है, उसके अपने अनुभवों द्वारा प्रमाणित होता है, जैसे 'मैं आनंदित हूँ', 'मैं दुखी हूँ' आदि। वह स्वयं उन कार्यों को अपनाता है जो वास्तव में उसके नहीं हैं, बल्कि अंतःकरण के हैं।
संशय: चूँकि जीव परिवर्तनशील है, तो वह 'साक्षी-स्वरूप आत्मा' कौन है जो जीव से भिन्न है? उसके क्या लक्षण हैं? उसके अस्तित्व का प्रमाण क्या है? उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
स्पष्टीकरण: साक्षी अपरिवर्तनीय आधार है। वही आत्मा है, जो सत्-चित्-आनंद स्वरूप है और आकाश की तरह सर्वव्यापक है। वही आत्मा अंतःकरण में जीव के रूप में प्रवेश कर सांसारिक अस्तित्व के अधीन हो जाती है। इस दिव्य आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण सभी वेदांत शास्त्र देते हैं। वास्तव में वही चेतना है जो चिदाभास (मूल चेतना का अंतःकरण में प्रतिबिंब) की विभिन्न अवस्थाओं को जानती है और उन अवस्थाओं का अनुभव करती है।
यह चेतना कभी जाग्रत होती है, कभी स्वप्न देखती है, और कभी अज्ञान के कारण गहरी निद्रा में लीन हो जाती है। कभी सुख का अनुभव करती है, कभी दुःख और कभी उदासीन रहती है। यही चेतना, जो जीव की अवस्थाओं के इन विभिन्न रूपों को साक्षी के रूप में जानती है, वही आत्मा है। वही आत्मा तीनों अवस्थाओं का साक्षी मानी जानी चाहिए।
संशय: आत्मा स्वयं को अपरिवर्तनीय कैसे जानती है?
स्पष्टीकरण: जैसे कोई व्यक्ति अपने चेहरे की सुंदरता को सीधे नहीं देख सकता, लेकिन दर्पण की सहायता से देख सकता है, वैसे ही आत्मा अपनी अपरिवर्तनीय प्रकृति को अंतःकरण में अपने प्रतिबिंब के माध्यम से जानती है। जैसे न तो दर्पण और न ही उसमें प्रतिबिंबित छवि वास्तविक चेहरे को जान सकते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण और उसमें प्रतिबिंबित आत्मा, जिसे चिदाभास कहा जाता है, आत्मा को नहीं जान सकते।
संशय: फिर आत्मा को कौन जानता है?
स्पष्टीकरण: आत्मा को कोई अन्य नहीं जान सकता, क्योंकि वही द्रष्टा है और शेष सब दृश्य हैं। आत्मा कोई बाह्य वस्तु नहीं है जिसे कोई अन्य जान या देख सके, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशस्वरूप है।
संशय: क्या इसे और स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है?
स्पष्टीकरण: हाँ। उदाहरण के लिए, एक घड़ा जिसे कोई व्यक्ति देख रहा है, वह देखने वाले को नहीं जान सकता, लेकिन देखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने अस्तित्व से अवगत होता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान है। जैसे दसवें व्यक्ति के खो जाने की कथा में, वह दसवाँ व्यक्ति, जिसे मृत मान लिया गया था, अंततः स्वयं को ही दसवाँ व्यक्ति जान लेता है, परंतु अन्य नौ लोग उसे नहीं जान सकते। उसी प्रकार, आत्मा, जिसे 'अज्ञात' या 'अदृश्य' माना जाता है, स्वयं अनुभव स्वरूप होने के कारण, मन, बुद्धि आदि द्वारा जानी नहीं जा सकती। इस निष्कर्ष को प्रमाणों की सहायता से भली-भाँति समझना चाहिए।
संशय: प्रमाण या प्रामाणिकता का क्या अर्थ है?
स्पष्टीकरण: प्रमाण सत्य ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। यह चार प्रकार के होते हैं:
1. प्रत्यक्ष (Pratyaksha) प्रमाण - प्रत्यक्ष अनुभव या इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान।
2. अनुमान (Anumana) प्रमाण - तर्क और संकेतों के आधार पर निष्कर्ष निकालना।
3. उपमान (Upamana) प्रमाण - तुलना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना।
4. शब्द (Sabda) प्रमाण - किसी विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्रों के कथन द्वारा प्राप्त ज्ञान।
इसके अतिरिक्त चार और प्रमाण माने जाते हैं:
5. अर्थापत्ति (Arthapatti) प्रमाण - किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्व जानकारी से अनुमान लगाना।
6. संभाव (Sambhava) प्रमाण - किसी तथ्य की संभावना के आधार पर उसे मान लेना।
7. ऐतिह्य (Aitihya) प्रमाण - परंपरागत मान्यताओं और इतिहास के आधार पर प्रमाणित ज्ञान।
8. अनुपलब्धि (Anupalabdhi) प्रमाण - किसी वस्तु की अनुपस्थिति से उसके अस्तित्व का निष्कर्ष निकालना।
हालाँकि, गहराई से अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि ये अंतिम चार प्रमाण पहले चार में ही समाहित हैं। कुछ वेदांती प्रमाणों की संख्या छह मानते हैं:
1. प्रत्यक्ष,
2. अनुमान,
3. उपमान,
4. शब्द,
5. अर्थापत्ति,
6. अनुपलब्धि।
विभिन्न दर्शनों में प्रमाणों को लेकर मतभेद:
● चार्वाक मत केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मान्यता देता है।
● बौद्ध और वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को मानते हैं।
● सांख्य और योग दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं।
● न्याय दर्शन इनमें उपमान को भी सम्मिलित करता है।
● मीमांसा के प्रभाकर संप्रदाय में अर्थापत्ति भी सम्मिलित की जाती है।
● वेदांत और भट्ट मीमांसा छह प्रमाणों को मानते हैं।
● पुराणिक विचारधारा संभाव और ऐतिह्य को भी प्रमाण के रूप में जोड़ती है।
प्रमुख चार प्रमाणों की व्याख्या:
1. प्रत्यक्ष प्रमाण:
○ 'अक्ष' का अर्थ 'इंद्रिय' है।
○ जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है।
○ उदाहरण: आँखों से किसी घट (घड़ा) को देखना।
2. अनुमान
प्रमाण:
○ किसी विशेष लक्षण के आधार पर किसी वस्तु के अस्तित्व का अनुमान लगाना।
○ उदाहरण: धुएँ को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना।
3. उपमान
प्रमाण:
○ किसी ज्ञात वस्तु के आधार पर किसी अन्य वस्तु को समझना।
○ उदाहरण: खच्चर को घोड़े के समान मानकर उसकी विशेषताओं को समझना।
4. शब्द
प्रमाण:
○ किसी विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्रों द्वारा दी गई जानकारी।
○ उदाहरण: 'तत्त्वमसि' (तू वही है)।
आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण: आत्मा इंद्रियों से परे है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण उस पर लागू नहीं होता। आत्मा अविभाज्य है, इसलिए अनुमान प्रमाण भी लागू नहीं होता। आत्मा अद्वितीय है, इसलिए उपमान प्रमाण भी नहीं चलता। इस कारण आत्मा का प्रमाण केवल शब्द प्रमाण से ही संभव है।
विश्वसनीय व्यक्ति के कथन को शब्द प्रमाण माना जाता है। एक विश्वसनीय व्यक्ति वह होता है जो सदा सत्य बोलता है। अतः शास्त्रों में दिए गए कथन, जो परमात्मा के वचन हैं, आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण हैं।
जैसे एक संन्यासी किसी आगंतुक को देखता है लेकिन उसकी स्थिति और क्रियाएँ उसे प्रभावित नहीं करतीं, वैसे ही आत्मा भी जीव के विभिन्न अवस्थाओं और कर्मों की साक्षी होती है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। जो व्यक्ति शास्त्रों के आधार पर आत्मा को शुद्ध, साक्षी, निर्गुण और अचल चेतना रूप में समझ लेता है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है।
इसलिए, आत्मा के बारे में प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांत शास्त्रों को स्वीकार कर आत्मा के साक्षी-स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए।
वर्णक 10
आत्मा पाँच कोशों से परे है
इस अध्याय में आत्मा के पाँच कोशों से परे होने की चर्चा की गई है। ये पाँच कोश निम्नलिखित हैं:
1. अन्नमय कोश (भौतिक कोश)
2. प्राणमय कोश (प्राणिक कोश)
3. मनोमय कोश (मानसिक कोश)
4. विज्ञानमय कोश (बौद्धिक कोश)
5. आनंदमय कोश (आनंद कोश)
1. अन्नमय कोश: यह स्थूल शरीर है। यह शुक्र और अंडाणु से उत्पन्न होता है, जो स्वयं अन्न (भोजन) के रूपांतरण मात्र हैं। यह षड्भाव विकारों (छह परिवर्तनों) के अधीन होता है:
● अस्तित्व (अस्ति)
● जन्म (जयते)
● वृद्धि (वर्धते)
● परिवर्तन (परिणमते)
● क्षय (अपक्षीयते)
● मृत्यु (विनश्यति)
यह भोजन द्वारा पोषित होता है।
2. प्राणमय कोश: यह पाँच प्राणों और पाँच कर्मेंद्रियों (क्रियात्मक इंद्रियों) के योग से बना होता है।
3. मनोमय कोश: यह मन और पाँच ज्ञानेंद्रियों (ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियों) के संयोग से बनता है।
4. विज्ञानमय कोश: यह भी पाँच ज्ञानेंद्रियों से बनता है, परंतु इसमें बुद्धि (विवेक) का समावेश होता है।
5. आनंदमय कोश: यह केवल अज्ञान होता है, जिसमें प्रिय (अपेक्षित आनंद), मोद (प्राप्ति से उत्पन्न आनंद) और प्रमोद (भोग के समय का आनंद) जुड़े होते हैं। ये तीन अवस्थाएँ क्रमशः किसी प्रिय वस्तु को देखने, उसे प्राप्त करने और उसके उपभोग से उत्पन्न सुख से संबंधित होती हैं।
जिस प्रकार म्यान तलवार को, एक अलंकरण पेटी शिवलिंग की मूर्ति को, फल का छिलका आम के फल को, और कमीज मनुष्य को ढकती है, वैसे ही पाँच कोश आत्मा को आवृत करते हैं। इसलिए इन्हें कोश कहा जाता है।
संदेह:- जबकि तलवार आदि के मामले में, वे और उनके आवरण अलग-अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, वही बात कोशों के बारे में नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनका आत्मा से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और इस कारण वे उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के आवरणों से पूरी तरह भिन्न हैं। फिर पंचकोशों में आत्मा को आच्छादित करने की शक्ति कैसे हो सकती है?
स्पष्टीकरण:- बादल सूर्य की किरणों के परिवर्तन का ही परिणाम होते हैं, फिर भी वे सूर्य को ढक लेते हैं। धुआँ अग्नि पर ही निर्भर होता है, फिर भी वह अग्नि को आच्छादित कर सकता है। इसी प्रकार, यद्यपि पंचकोश केवल आत्मा के कारण ही अस्तित्व में होते हैं, फिर भी उनमें आत्मा को ढकने की शक्ति होती है, और इसलिए उन्हें उचित रूप से 'कोश' या आवरण कहा जाता है।
अब हम देखेंगे कि आत्मा पंचकोशों से कैसे परे है। यद्यपि 'तलवार' जैसे शब्दों का प्रयोग सामान्यतः उनके म्यान सहित किया जाता है, फिर भी तलवार अपने म्यान से भिन्न होती है। इसी प्रकार, यद्यपि सांसारिक लोग आत्मा और पंचकोशों को एक ही शब्द 'आत्मा' से संदर्भित करते हैं, फिर भी आत्मा पंचकोशों से परे होती है।
संशय: चूँकि सांसारिक चर्चा में आत्मा और पाँच कोशों को समान माना जाता है, तो उन्हें कम से कम संबंधित वस्तुएँ तो कहा ही जाना चाहिए। फिर इन्हें असंबद्ध कैसे कहा जा सकता है?
स्पष्टीकरण: संबंध कई प्रकार के होते हैं। न्याय दर्शन में दो प्रकार के संबंध माने गए हैं:
1. समवाय-संबंध (अविभाज्य अंतर्निहित संबंध) - यह संपूर्ण और उसके भागों, विशेषण और उसके गुणों, कर्ता और उसकी क्रिया, जाति और प्रजाति, पदार्थ और उसके भेद के बीच पाया जाता है। यह संबंध आत्मा और पाँच कोशों के बीच नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी संपूर्ण और उसके अवयव नहीं माने जाते।
2. संयोग-संबंध (संपर्क द्वारा संबंध) - जैसे लकड़ी और ढोल के बीच संबंध होता है, परंतु आत्मा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, जबकि कोश पंचमहाभूतों के रूपांतरण हैं। इसलिए इनके बीच यह संबंध भी संभव नहीं है।
हालाँकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आत्मा और पाँच कोशों के बीच कोई संबंध नहीं है। इनके बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, जिसे अध्यास-संबंध (आरोपित संबंध) कहा जाता है। जैसे रस्सी पर साँप का भ्रम, सीप में चाँदी का भ्रम, खंभे पर भूत का भ्रम, या आकाश का नीला रंग प्रतीत होना, वैसे ही आत्मा और पाँच कोशों के बीच यह संबंध देखा जाता है। यह आरोपित संबंध एकतरफा न होकर पारस्परिक होता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि आत्मा और अहंकार दोनों एक साथ 'मैं' की भावना के विषय बनते हैं।
अन्नमय कोश और आत्मा के बीच आरोपित संबंध:
वाक्य जैसे - 'मैं पुरुष हूँ', 'मैं देवता हूँ', 'मैं स्त्री हूँ', 'मैं जन्मा हूँ', 'मैं वृद्ध हूँ', 'मैं ब्राह्मण हूँ', 'मैं क्षत्रिय हूँ', 'मैं व्यापारी हूँ', 'मैं संन्यासी हूँ', 'मैं आंध्र प्रदेश का हूँ', 'मैं तमिलनाडु का हूँ', 'मैं कर्नाटका से हूँ', आदि स्पष्ट रूप से अन्नमय कोश के गुणों और अवस्थाओं का आत्मा पर आरोपण दर्शाते हैं।
इसी प्रकार, आत्मा के सत्-चित्-आनंद (अस्तित्व, प्रकाश और आनंद) गुणों का अन्नमय कोश पर आरोपण इस प्रकार होता है - 'मेरा शरीर है', 'यह चमकता है', 'यह मुझे प्रिय है'। वास्तव में अस्तित्व, प्रकाश और प्रियता आत्मा के गुण हैं, परंतु ये शरीर पर आरोपित हो जाते हैं।
प्राणमय कोश और आत्मा के बीच आरोपित संबंध:
वाक्य जैसे - 'मैं भूखा हूँ', 'मैं प्यासा हूँ', 'मैं शक्तिशाली हूँ', 'मैं कर्मशील हूँ', 'मैं वक्ता हूँ', 'मैं चलने वाला हूँ', 'मैं देने वाला हूँ', 'मैं मलत्यागी हूँ', 'मैं मूक हूँ', 'मैं लंगड़ा हूँ', 'मैं नपुंसक हूँ', आदि स्पष्ट रूप से प्राणमय कोश के गुणों का आत्मा पर आरोपण दिखाते हैं।
इसी प्रकार, 'मेरा प्राण है', 'यह चमकता है', 'यह मुझे प्रिय है' - यह आत्मा के गुणों का प्राणमय कोश पर आरोपण दर्शाते हैं।
मनोमय कोश और आत्मा के बीच आरोपित संबंध:
वाक्य जैसे - 'मैं विचारक हूँ', 'मैं संदेह करता हूँ', 'मैं शोक करता हूँ', 'मैं मोहग्रस्त हूँ', 'मैं लोभी हूँ', 'मैं कंजूस हूँ', 'मैं श्रोता हूँ', 'मैं अनुभव करता हूँ', 'मैं देखता हूँ', 'मैं स्वाद लेता हूँ', 'मैं सूँघता हूँ', 'मैं बहरा हूँ', 'मैं अंधा हूँ' आदि स्पष्ट रूप से मनोमय कोश के गुणों का आत्मा पर आरोपण दर्शाते हैं।
इसी प्रकार, 'मेरा मन है', 'यह चमकता है', 'यह मुझे प्रिय है' - यह आत्मा के गुणों का मन पर आरोपण दर्शाते हैं।
विज्ञानमय कोश और आत्मा के बीच आरोपित संबंध:
वाक्य जैसे - 'मैं कर्ता हूँ', 'मैं बुद्धिमान हूँ', 'मैं चतुर हूँ', 'मेरी धारणा शक्ति तेज है', 'मैं पुनर्जन्म को प्राप्त होता हूँ', 'मैं प्रेमी हूँ', 'मैं द्वेषी हूँ', 'मैं विद्यार्थी हूँ', 'मैं विद्वान हूँ', 'मैं वैराग्यवान हूँ', 'मैं भक्त हूँ', 'मैं उपासक हूँ', 'मैं ज्ञानी हूँ' आदि स्पष्ट रूप से विज्ञानमय कोश के गुणों का आत्मा पर आरोपण दर्शाते हैं।
इसी प्रकार, 'मेरा बुद्धि है', 'यह चमकती है', 'यह मुझे प्रिय है' - यह आत्मा के गुणों का विज्ञानमय कोश पर आरोपण दर्शाते हैं।
आनंदमय कोश और आत्मा के बीच आरोपित संबंध:
वाक्य जैसे - 'मैं भोगी हूँ', 'मैं आनंदित हूँ', 'मैं संतुष्ट हूँ', 'मैं पवित्र हूँ', 'मैं सक्रिय हूँ', 'मैं जड़ हूँ', 'मैं मूर्ख हूँ', 'मैं शून्य हूँ', 'मैं भ्रमित हूँ', 'मैं विवेकहीन हूँ', आदि स्पष्ट रूप से आनंदमय कोश के गुणों का आत्मा पर आरोपण दिखाते हैं।
इसी प्रकार, 'मेरा अज्ञान है', 'यह अनुभव किया जाता है', 'उस अवस्था में सुख है' - यह आत्मा के गुणों का आनंदमय कोश पर आरोपण दर्शाते हैं।
इस प्रकार, परस्पर आरोपण (अन्योन्य-अध्यास) सिद्ध होता है, जिसमें पाँच कोशों के गुण आत्मा पर आरोपित होते हैं और आत्मा के गुण पाँच कोशों पर आरोपित होते हैं।
संशय: कहा गया है कि आत्मा और पाँच कोशों के बीच संबंध अन्योन्य-अध्यास (पारस्परिक आरोपण) का है। यह क्यों होता है?
स्पष्टीकरण: यह सही ज्ञान के अभाव के कारण उत्पन्न होता है कि 'यह आत्मा है, और ये पाँच कोश हैं'। आत्मा और कोशों के बीच भेद न कर पाने की यह अविवेकता ही इस पारस्परिक आरोपण का कारण है।
संशय: आत्मा और पाँच कोशों में भेद कैसे किया जाए और उन्हें अलग-अलग कैसे पहचाना जाए?
स्पष्टीकरण: जिस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में गाय, संतान, मित्र, पत्नी, घर, धन, वस्त्र आदि में 'मेरा' भाव रखते हैं, उसी प्रकार पाँच कोशों के संदर्भ में भी हम कहते हैं - 'यह मेरा शरीर है', 'यह मेरा प्राण है', 'यह मेरा मन है', 'यह मेरी बुद्धि है', 'यह मेरा अज्ञान है'। चूँकि 'यह' और 'मेरा' की अवधारणा बुद्धि के लिए ज्ञेय वस्तुएँ हैं, इसलिए भौतिक शरीर आदि के रूप में स्थित ये पाँच कोश आत्मा नहीं हो सकते। जैसे गाय आदि आत्मा से भिन्न हैं, वैसे ही ये कोश भी आत्मा से पूर्णतः भिन्न हैं। यही तर्क लेकर निष्कर्ष निकालना चाहिए। श्रुति भी कहती है कि 'आत्मा शरीर रहित है'। व्यावहारिक अनुभव के दृष्टिकोण से स्थिति स्पष्ट है।
जिस प्रकार गाय आदि के विभिन्न परिवर्तन, जैसे वृद्धि और क्षय, उनके स्वामी को प्रभावित नहीं करते, उसी प्रकार कोशों के परिवर्तन आत्मा को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि आत्मा केवल उनका साक्षी है।
संशय: ऊपर दिए गए उदाहरणों में गाय आदि को आसानी से अलग माना जा सकता है, क्योंकि वे स्वामी से भिन्न और बाह्य हैं। लेकिन कोश तो आंतरिक होते हैं, इसलिए उनका वस्तुनिष्ठ और भिन्न अस्तित्व समझना कठिन है। साथ ही, पाँच कोश स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं देखे जाते, बल्कि वे आत्मा के साथ उतने ही एकीकृत प्रतीत होते हैं, जितना कि तप्त लोहे में गर्मी। इस प्रकार, उदाहरण और प्रत्यक्ष विषय में सामंजस्य नहीं लगता। तो हम कैसे विश्वास करें कि पाँच कोश आत्मा से भिन्न हैं?
स्पष्टीकरण: नेत्र केवल बाहरी दृष्टि का साधन हैं, जबकि बुद्धि सूक्ष्म दृष्टि का साधन है। जो वस्तुएँ बाहरी इंद्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं जानी जा सकतीं, उन्हें आंतरिक साधनों से जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, वीणा के तारों से उत्पन्न ध्वनि, उष्ण जल में छिपी हुई गर्मी, और पुष्प से निकटता में स्थित सुगंध को सामान्य दृष्टि से पृथक रूप में देख पाना कठिन होता है। लेकिन एक प्रबुद्ध व्यक्ति अपनी आंतरिक बुद्धि से इन्हें अलग-अलग समझ सकता है। इसी प्रकार, यह कहना कि दूध और जल को पृथक करना कठिन है, यह उनकी भिन्नता को नकारने का प्रमाण नहीं हो सकता। हंस (पौराणिक राजहंस) दूध को जल से अलग कर सकता है। इसी तरह, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म और तेज है, वे आत्मा और पाँच कोशों के भेद को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।
अब हम उन निष्कर्षों की ओर ध्यान देते हैं जो सत्य के ज्ञाताओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। वास्तव में, अब तक पाँच कोशों और उनके स्वरूप की चर्चा केवल एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति के सापेक्षिक दृष्टिकोण से की गई थी, जो देश, काल और स्थिति की चेतना में बँधा हुआ होता है। लेकिन परम वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखें, तो आत्मा में कोई कोश आदि होते ही नहीं। जैसे रस्सी में दिखने वाला साँप, सीप में चाँदी, खंभे में भूत, और आकाश में नीला रंग केवल भ्रांतियाँ होती हैं, वैसे ही पाँच कोश भी आत्मा पर आरोपित भ्रांतियाँ मात्र हैं।
यह सर्वमान्य तथ्य है कि सभी आरोपित वस्तुएँ तीनों कालों में अवास्तविक होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे नेत्र दोष होने पर दो चंद्रमा का दिखना असत्य होता है। इसलिए निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाँच कोश भी केवल आरोपण हैं और वास्तव में असत्य हैं।
संशय: जब आधारभूत सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आरोपित वस्तुएँ जैसे साँप, चाँदी आदि लुप्त हो जाते हैं। लेकिन आत्मा के ज्ञान के बाद भी पाँच कोश समाप्त नहीं होते, बल्कि वे अनुभव में बने रहते हैं। तो फिर उन्हें केवल आरोपण कैसे कहा जा सकता है?
स्पष्टीकरण: वास्तविकता तीन प्रकार की होती है:
1. व्यवहारिक सत्ता (Vyavaharika Satta) - व्यावहारिक जगत में जो कुछ भी अनुभव किया जाता है, वह इस श्रेणी में आता है।
2. प्रतीतिमान सत्ता (Pratibhasika Satta) - जो केवल भ्रमजन्य अनुभव होता है, जैसे सीप में चाँदी का आभास।
3. परमार्थिक सत्ता (Paramarthika Satta) - परम सत्य, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है।
सृष्टि भी दो प्रकार की होती है:
1. जीव-सृष्टि (Jiva-Srishti) - जो जीव के व्यक्तिगत भ्रम से उत्पन्न होती है, जैसे मृग-मरीचिका।
2. ईश्वर-सृष्टि (Isvara-Srishti) - जो ईश्वर द्वारा निर्मित वास्तविक जगत है।
सभी आरोपण, जैसे सीप में चाँदी देखना आदि, वास्तव में जीव-सृष्टि का भाग होते हैं और प्रतीतिमान सत्ता में आते हैं। लेकिन आकाश, पृथ्वी आदि, जो इस जगत के आधारभूत तत्व हैं, व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत आते हैं और ईश्वर-सृष्टि का भाग होते हैं। जो 'परम सत्य' है, वही इन सबका आधार है। केवल वही शाश्वत है। व्यावहारिक सत्ता तब तक रहती है जब तक सांसारिक कर्म चलते रहते हैं। प्रतीतिमान सत्ता तब तक रहती है जब तक भ्रम बना रहता है।
अगर व्यवहारिक सत्ता भी ज्ञान प्राप्ति के साथ समाप्त हो जाए, तो संसार में मुक्त व्यक्तियों का अस्तित्व ही असंभव हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि संसार में कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होगा जो शिष्यों को आत्मज्ञान प्रदान कर सके। गुरु-शिष्य परंपरा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ज्ञानियों के लिए व्यवहार की अनुपस्थिति होगी और अज्ञानियों के लिए शिक्षा देने की असमर्थता होगी।
अंतिम निष्कर्ष यह है कि जैसे घड़ा केवल मिट्टी पर आरोपित होता है, लेकिन जब तक कुम्हार का प्रयास जारी रहता है, तब तक वह बना रहता है, वैसे ही पाँच कोशों का आत्मा पर आरोपण, उनके अवास्तविक होने का ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी, प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने तक बना रहता है। परंतु यह केवल जल चुके कपड़े की तरह होता है, जो दिखता तो है, लेकिन उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता।
अतः
आगे की चर्चाएँ अनावश्यक होंगी। इसलिए सिद्धांत को ही
सुनना उचित है। जिस प्रकार
जब घड़े का नाम और
रूप मिट जाता है, तब केवल मिट्टी ही
शेष रहती है,
जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसी प्रकार जब आत्मा
पर आरोपित पाँच कोशों की
भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती हैं,
तब केवल सत्-चित्-आनंद रूपी आत्मा
ही अविनाशी सत्य के रूप
में बनी रहती है। जो
व्यक्ति इस प्रकार आत्मा का
साक्षात्कार करता
है, वही आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी होता है। वही व्यक्ति
देह से परे मोक्ष (विदेहमुक्ति) का अनुभव करता
है। यही उपनिषदों का निरंतर संदेश है।
अध्याय -11
आत्मा सत्-चित्-आनंद स्वरूप है
आत्मा की चौथी विशेषता, अर्थात् सत्-चित्-आनंद (अस्तित्व-चेतना-आनंद) को इस अध्याय में समझाया गया है।
संशय: आत्मा का अस्तित्व (सत्) क्या है, इसका चेतना (चित्) स्वरूप क्या है, और इसका आनंद (आनंद) स्वरूप क्या है?
स्पष्टीकरण: सत् या अस्तित्व वह है जो तीनों कालों (अतीत, वर्तमान, भविष्य) में कभी भी नष्ट नहीं होता और किसी भी वस्तु से अप्रभावित रहता है। यह गुण आत्मा में निहित है।
संशय: इसका प्रमाण क्या है?
स्पष्टीकरण: शास्त्र (श्रुति) इसका प्रमाण हैं। वे घोषित करते हैं: "इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले केवल सत् ही विद्यमान था।" और "आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ।" इसके अतिरिक्त, अनुभव (अनुभवजन्य प्रमाण) भी इसका समर्थन करता है।
● एक धनवान व्यक्ति सोचता है: "पिछले जन्म में मैंने योग्य व्यक्तियों को दान किया होगा, इसलिए इस जन्म में मैं समृद्ध हूँ। यदि मैं इस जन्म में भी दान करूँ, तो अगले जन्म में भी समृद्ध रहूँगा।"
● एक गरीब व्यक्ति सोचता है: "पिछले जन्म में मैंने कुछ दान नहीं किया, इसलिए मैं अब गरीब हूँ। यदि मैं इस जन्म में भी कुछ नहीं दूँगा, तो अगले जन्म में भी मेरी स्थिति यही रहेगी।"
● एक कर्मकांडी व्यक्ति तर्क करता है: "पिछले जन्म में मैंने पुण्य कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में मैं धार्मिक कार्य कर पा रहा हूँ। यह मुझे अगले जन्म में स्वर्ग में देवता बनने का अवसर देगा।"
● एक भक्त सोचता है: "पिछले जन्म में मैंने भगवान की उपासना की होगी, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में मेरे भीतर भक्ति उत्पन्न हुई है। इससे अगले जन्म में मुझे वैकुंठ आदि स्वर्गीय लोकों में आनंद प्राप्त होगा।"
● एक आध्यात्मिक साधक इस प्रकार सोचता है: "असंख्य पूर्व जन्मों में मैंने अच्छे कर्म किए और उनके फलों को भगवान को समर्पित किया। इस कारण मुझे इस जन्म में साधन-चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, शमादि षट्संपत्ति, और मुमुक्षा), गुरु, श्रवण आदि प्राप्त हुए और अब मैं आत्म-साक्षात्कार के समीप हूँ। अब मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं है। मैंने वह सब कर लिया है जो मुझे करना था।"
इन सभी विचारों में एक सामान्य तत्व है - तीनों कालों में व्यक्ति अपने अस्तित्व की निरंतरता का अनुभव करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नाश केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। अतः आत्मा सर्वदा विद्यमान रहती है और इसे सत् (शुद्ध अस्तित्व) कहा जाता है।
संशय: शास्त्र और अनुभव के आधार पर आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि की गई, परंतु तर्क (युक्ति) का क्या?
स्पष्टीकरण: केवल यह विचार करना कि "क्या हम अस्तित्व में हैं?" इस प्रश्न का उत्तर बिना किसी संदेह के मिलता है कि "हाँ, हम सभी विद्यमान हैं।" यह प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। इसी प्रकार, यह सिद्ध करने के लिए कि हम शरीरधारी हैं, अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
संशय: यह शरीरधारण कैसे हुआ?
स्पष्टीकरण: यह अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि यह कर्मों के कारण हुआ है।
संशय: क्या यह कर्म स्वयं किए गए हैं या किसी और ने किए हैं?
स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट है कि कर्म स्वयं द्वारा किए गए हैं। अन्यथा, एक व्यक्ति के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी अन्य को स्वर्ग प्राप्त हो सकता था। उदाहरण के लिए, यदि किसी ब्राह्मण ने यज्ञ किया हो, और उसका फल किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाए, तो यह अनुचित होगा। इसी प्रकार, यदि प्राचीन काल में महर्षि शुकदेव ने समाधि का अनुभव किया, तो उसके कारण हम सभी मुक्त हो चुके होते। अतः यह सिद्ध होता है कि केवल स्वयं के कर्मों का ही फल मिलता है।
संदेह: क्या वे कर्म, जिन्होंने इस वर्तमान शरीर को उत्पन्न किया, इस जन्म में किए गए थे या पूर्व जन्मों में?
स्पष्टीकरण: इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान शरीर केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। इसके विपरीत किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना अविवेकपूर्ण होगा, क्योंकि केवल वे कर्म जो जन्म से पहले किए गए हैं, शरीर को उत्पन्न कर सकते हैं।
संदेह: क्या हम उस पूर्व जन्म में अस्तित्व में थे जिसमें ये कर्म किए गए थे?
स्पष्टीकरण: निश्चय ही हम अस्तित्व में थे, क्योंकि जो कभी अस्तित्व में नहीं था, वह कोई भी कर्म कर ही नहीं सकता।
संदेह: क्या तब हमारे पास भी एक शरीर था?
स्पष्टीकरण: निश्चित रूप से ऐसा ही रहा होगा; अन्यथा हम कर्म कैसे कर सकते थे?
संदेह: क्या वह शरीर उस जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम था या उससे भी पहले के जन्मों का?
स्पष्टीकरण: इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वह भी पिछले जन्मों का परिणाम था। इस प्रकार, यदि हम शरीर और उसके कारण, अर्थात् कर्मों की प्रकृति की जाँच करते जाएँ, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह एक अनादि श्रृंखला है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। यही कारण है कि आत्मा, जो हमारे शरीर और कर्मों का आधारभूत तत्व है, अनादि और स्वयं के स्वभाव से विद्यमान होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश। इस प्रकार, तर्क-प्रणालियों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि आत्मा का अस्तित्व न केवल भूतकाल में था, बल्कि वर्तमान में भी है।
उसी प्रकार, तर्क के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि आत्मा भविष्य में भी विद्यमान रहेगी। चूँकि बिना श्रवण (शास्त्रों का सुनना), मनन (विचार करना) आदि में संलग्न हुए भी हमने पूर्व जन्मों में इच्छाओं के प्रभाव से विभिन्न कर्म किए, जिससे यह वर्तमान जन्म और शरीर उत्पन्न हुए, उसी प्रकार इस जन्म में किए गए कर्म भविष्य के जन्म का कारण बनेंगे, और उस जन्म में किए गए कर्म फिर से अगले जन्म का कारण बनेंगे। इस प्रकार, यदि हम कर्म और जन्मों की प्रकृति का गहराई से विश्लेषण करें, तो हम पाएँगे कि जन्म और कर्मों की यह श्रृंखला अनंत रूप से चलती रहती है। जब तक ज्ञान के द्वारा कर्मों का नाश नहीं हो जाता, तब तक शरीर का अंत नहीं होगा।
आत्मा, जिससे यह दोनों (शरीर और कर्म) संबंधित हैं, सृष्टि और शरीर के नाश के दौरान भी निरंतर विद्यमान रहती है। यह विभिन्न रूपों में जन्म लेती हुई सुख-दुख का अनुभव करती रहती है, एक तिनके से लेकर ब्रह्मा तक के रूप में, जब तक कि परम ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। जब ज्ञान का प्रकाश उदित होता है, तब अज्ञान, इच्छाएँ और कर्म नष्ट हो जाते हैं और आत्मा अपने ही आनंद में स्थित हो जाती है, जिसे शरीर के बंधन से मुक्त मोक्ष कहा जाता है। तब आत्मा का विनाश भविष्य में भी असंभव हो जाता है। इस प्रकार, तर्क द्वारा यह निश्चित रूप से सिद्ध किया जाता है कि आत्मा सदा विद्यमान रहती है।
इस प्रकार, श्रुति (शास्त्र), युक्ति (तर्क) और अनुभूति (प्रत्यक्ष अनुभव) के द्वारा यह सिद्ध होता है कि आत्मा तीनों कालों—भूत, वर्तमान और भविष्य—में बिना किसी परिवर्तन और विनाश के विद्यमान रहती है, चाहे असंख्य ब्रह्मांडों की रचना और विनाश होते रहें। इसलिए, उत्पत्ति, स्थिति और लय केवल ब्रह्मांड से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। संक्षेप में, आत्मा सत् या शुद्ध अस्तित्व है, क्योंकि यह सदा अविनाशी रूप में एक ही सत्ता के रूप में बनी रहती है।
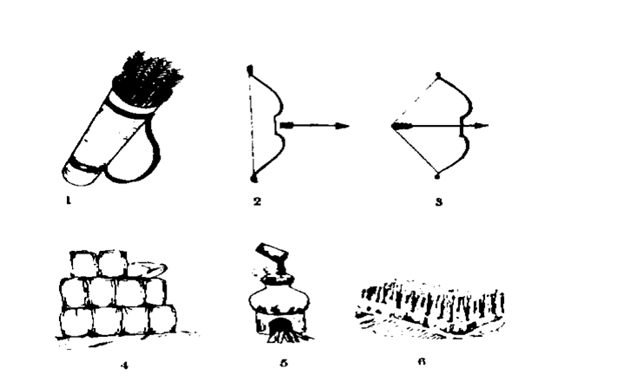
चित्र 13: तीन प्रकार के कर्म
I. संचित कर्म (1 व 4): तीर और खाद्यान्न के भंडार के समान।
II. प्रारब्ध कर्म (2 व 5): धनुष से छूटा हुआ तीर और भंडार से दिन भर के लिए निकाला गया अनाज।
III. आगामी कर्म (3 व 6): तीर चलाने के लिए तैयार रखा गया तीर और भविष्य के लिए नई फसल उगाने के समान।
संदेह: आत्मा का चित् (शुद्ध चेतना) स्वरूप होने का क्या प्रमाण है?
स्पष्टीकरण: वह सत्ता जो न केवल जड़ वस्तुओं को प्रकाशित करती है, बल्कि स्वयं को भी बिना किसी बाहरी साधन के सूर्य की भाँति प्रकाशित करती है, उसे चित् स्वरूप कहा जाता है। यह चित् स्वरूप आत्मा में पाया जाता है। गहरे अंधकार में भी आत्मा स्वयं को प्रकाशित करती है। इसके अलावा, आत्मा बिना किसी बाहरी तत्व की सहायता के शरीर की विभिन्न अवस्थाओं, जैसे बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि, तथा इन अवस्थाओं से जुड़े क्रियाकलापों को भी जानने में सक्षम होती है। इस प्रकार, आत्मा का चित् स्वरूप सिद्ध होता है।
संदेह: हम सर्वज्ञ नहीं हैं, और हमारा ज्ञान सीमित है। फिर हम सभी वस्तुओं को किस प्रकार प्रकाशित कर सकते हैं?
स्पष्टीकरण: ब्रह्मांड दो प्रकार का होता है—आंतरिक और बाह्य। हम दोनों को जानते हैं, लेकिन वे हमें कभी प्रकाशित नहीं कर सकते। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है—बाह्य ब्रह्मांड में रूप, गुण, ध्वनि, स्पर्श, रस और गंध सहित पंचमहाभूत, चौदह लोक और चार प्रकार के प्राणी आते हैं। हम इन सभी को उनके विभिन्न अंगों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड हमें प्रकाशित नहीं कर सकता। इस आत्मपरक जाँच के परिणामस्वरूप हम यह देख सकते हैं कि हमारी मूल प्रकृति बाह्य ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली सत्ता की है।
संदेह: हम आंतरिक ब्रह्मांड को किस प्रकार प्रकाशित करते हैं?
स्पष्टीकरण: आंतरिक ब्रह्मांड में शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, निर्णय, निद्रा, चेतना, सुख, दुख, इच्छा, घृणा, आदि आते हैं। इन सभी को हम जानते हैं, लेकिन वे हमें नहीं जानते। इस प्रकार, यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा ही चित् स्वरूप है।
संदेह: पहले यह कहा गया था कि चेतना किसी के द्वारा जानी नहीं जाती। लेकिन मन सभी चीजों को जानने में सक्षम प्रतीत होता है। फिर यह आत्मा को क्यों नहीं देख सकता?
स्पष्टीकरण: मन जन्म और मृत्यु के अधीन है; यह संकल्पों के रूप में कार्य करता है; यह सीमित है और पंचमहाभूतों से निर्मित है; यह इच्छाओं से प्रभावित होता है और स्मृति तथा विस्मृति के रूप में कार्य करता है। इसलिए यह जड़ है और स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसके अलावा, यह चेतना द्वारा ज्ञात होता है। तो फिर यह स्वयं-प्रकाशित आत्मा को कैसे जान सकता है? वास्तव में यह असंभव है।
संदेह: तब शास्त्रों में कहा गया यह वाक्य कि "इसे केवल मन द्वारा ही देखा जाना चाहिए" किस प्रकार समझा जाए?
स्पष्टीकरण: इसे शब्दशः नहीं समझना चाहिए। जैसे अग्नि में तपने के बाद सोना चमक उठता है, वैसे ही मन जब आत्मा से तादात्म्य स्थापित करता है, तो अज्ञान का पर्दा हट जाता है। तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्वयं प्रकाशित होती है। इस शास्त्रीय वाक्य का यही वास्तविक अर्थ है। इसलिए, यह आत्मा ही है जो मन को प्रकाशित करती है, न कि मन आत्मा को।
संदेह: आत्मा का आनंद स्वरूप क्या है?
स्पष्टीकरण: शाश्वत, असीम और सर्वोच्च सुख को आनंद कहा जाता है, और यही आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। फूल, चंदन, स्त्री आदि से प्राप्त सुख क्षणिक और सीमित होता है, इसलिए वह आत्मा का आनंद नहीं हो सकता। गहरी नींद की अवस्था में आनंद का अनुभव होता है, और इसलिए यह सिद्ध होता है कि आनंद आत्मा का स्वभाव है।
संदेह: गहरी नींद में केवल दुख का अभाव होता है, न कि आनंद का अनुभव। फिर इसे आनंद क्यों कहा जाता है?
स्पष्टीकरण: क्या यह सत्य नहीं कि जब कोई व्यक्ति गहरी नींद से जागता है, तो कहता है, "मैं सुखद अवस्था में था"? इसलिए यह स्पष्ट है कि गहरी नींद में आनंद का अनुभव होता है।
संक्षेप में, श्रुति (शास्त्र), तर्क और अनुभव के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आत्मा का स्वरूप सत्-चित्-आनंद है।
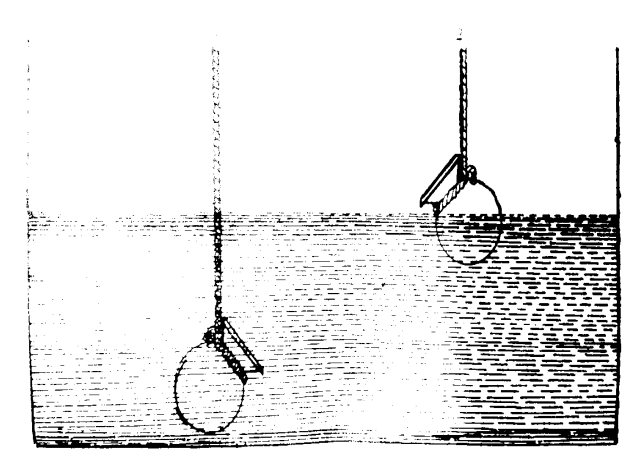
चित्र 14. (1) एक ऋषि और (2) एक आम आदमी की स्थिति।
वर्णक 12
आत्मा अविभाज्य परम सत्य है
इस अध्याय में गुरु ने शिष्य पर दया करके आत्मा के 'अविभाज्य परम' स्वरूप का रहस्य समझाया है।
शिष्य:-हे गुरुदेव! आपके महान आत्मा द्वारा पिछले ग्यारह अध्यायों में दिए गए निर्देशों के प्रवाह से, शरीर और पाँच कोशों में 'मैं' और 'मेरा' की धारणा गायब हो गई है। मुझे यह ज्ञान भी प्राप्त हो गया है कि मैं ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं हूँ, जो सत्-चित्-आनंद की प्रकृति का है और जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक और संदेह है। यह कहा गया है कि आत्मा सत्, चित् और आनंद की प्रकृति है। ये तीन शब्द जो तीन अलग-अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं, तीन अलग-अलग अर्थों को व्यक्त करते हैं। जब ऐसा है, तो ये तीन शब्द अविभाज्य परम पर कैसे लागू हो सकते हैं?
गुरु:-हे पुत्र! यह जान लें कि जब कोई इकाई देश, काल और पदार्थ की सीमाओं से रहित होती है, तब उसे अविभाज्य निरपेक्ष या अखंड कहा जाता है। उस निरपेक्ष ब्रह्म के लिए इन तीनों विशेषताओं का होना आवश्यक है। शिष्य:-ऐसी तीन-सूत्री परिभाषा का उद्देश्य या आवश्यकता क्या है? गुरु:-यदि निरपेक्ष को केवल देश की सीमाओं से परे कहा जाए, तो यह परिभाषा ईथरियल स्पेस पर भी समान रूप से लागू होने के कारण, जो सर्वव्यापी भी है, स्पष्ट रूप से बहुत व्यापक होगी। 'अतिव्याप्ति' नामक इस दोष को दूर करने के लिए, समय के संबंध में पारगमन को भी एक आवश्यक वस्तु के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। उस स्थिति में यह परिभाषा ईथर पर लागू नहीं होगी क्योंकि यह समय से बंधा हुआ है, अर्थात इसका एक उद्गम और एक अंत है। ये दोनों कारक, फिर से, स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि परिभाषा अब समय पर लागू होती है। क्योंकि, समय न तो देश से सीमित है, न ही अपने आप से, क्योंकि यह असंभव है कि यह अपने आप में परिबद्ध हो सके। इस कमी को पूरा करने के लिए परिभाषा में तीसरा कारक अर्थात् द्रव्य द्वारा सीमा भी शामिल की गई है। चूँकि समय से भिन्न तथा बाह्य पदार्थ भी हैं, इसलिए वह उनके द्वारा सीमित है। इसलिए तीसरे कारक अर्थात् द्रव्य के जुड़ने से किसी भी प्रकार का अतिव्यय नहीं होता। केवल ब्रह्म ही इन तीन सीमाओं के अधीन नहीं है, इसलिए ये तीनों विशेषताएँ ब्रह्म की ही बताई गई हैं। इन्हीं के द्वारा आत्मा को अविभाज्य निरपेक्ष जानना चाहिए।
शिष्य:-यदि अविभाज्य निरपेक्ष की ये तीन विशेषताएँ आत्मा में होतीं, तो सभी को उनका अनुभव होता। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी को यह कहते हुए पाते हैं कि 'मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं वहाँ नहीं खड़ा हूँ', जो स्थान द्वारा आत्मा की कंडीशनिंग को इंगित करता है। 'मैं उस वर्ष में पैदा हुआ था और मैं दस वर्ष बाद मर सकता हूँ' जैसे भाव आत्मा के काल द्वारा बंधे होने का संकेत देते हैं, और 'मैं ब्राह्मण नहीं हूँ', 'मैं क्षत्रिय नहीं हूँ' आदि भाव यह संकेत देते हैं कि आत्मा द्रव्य द्वारा भी सीमाओं से मुक्त नहीं है। इसलिए, यह कैसे कहा जाता है कि आत्मा इन तीन सीमाओं के अधीन नहीं है?
गुरु:-ग्यारहवें अध्याय में जब मैंने आपको आत्मा और अनात्मा के लक्षण समझाए थे, तब क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था कि 'आत्मा सर्वव्यापी है, अनात्मा सीमित है और सभी 'दृश्यमान' पदार्थ आरोपित हैं? इस स्पष्टीकरण के बावजूद, आपने अब आत्मा के लक्षणों के बारे में वही प्रश्न किया है। इसलिए मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या आप 'सच्चे' शिष्य हैं या केवल झगड़ालू विवादी हैं। यदि आप शिष्य हैं तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यदि आप मेरे विरोधी हैं, तो मुझे केवल धैर्यपूर्वक मौन रहना है, या क्रोध में आपको शाप देना है। बेशक, चूँकि मेरे शिष्य को दीक्षा के रूप में मेरा आशीर्वाद उस पर अपना प्रभाव डालता है, इसलिए बिना कहे ही यह निष्कर्ष निकलता है कि मेरे विरोधी पर भी श्राप का प्रभाव पड़ेगा। यह भी जान लो कि इस संसार में किसी को आशीर्वाद देने या श्राप देने की शक्ति में ब्रह्म के ज्ञाता और ईश्वर के बीच वास्तव में कोई अंतर नहीं है।
शिष्य: हे परम पावन गुरु! कृपया मुझे केवल अपनी कृपा के योग्य शिष्य के रूप में ही समझो। मैंने यह प्रश्न केवल संदेह के कारण आपसे पूछा है, कुतर्क या दुर्भावनापूर्ण तर्क के लिए नहीं।
गुरु:-तो मैं फिर से तुम्हें मामला समझाता हूँ। सुनो। स्थान, काल और पदार्थ की तीन सीमाएँ स्वाभाविक रूप से केवल शरीर पर लागू होती हैं, परिपूर्ण प्रत्यगत्मा या सर्व-पूर्ण ब्रह्म पर नहीं।
शिष्य: कैसे पता चले कि आत्मा में स्थान की कोई सीमा नहीं है?
गुरु: हम ऐसे कथनों का उल्लेख करते हैं जैसे 'बर्तन मौजूद है', 'कपड़ा मौजूद है', 'दीवार मौजूद है', 'अन्न भंडार मौजूद है', 'पृथ्वी मौजूद है', 'पानी मौजूद है', 'अग्नि मौजूद है', 'वायु मौजूद है', 'आकाश मौजूद है', आदि। इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म ब्रह्मांड दोनों ही उनके अस्तित्व पहलू के माध्यम से हमारे द्वारा अनुभव किए जाते हैं। इसलिए, अस्तित्व के रूप में आत्मा स्थान की सीमा के अधीन हुए बिना सर्वव्यापी है। तर्क-वितर्क की एक समान प्रक्रिया इस तथ्य को स्थापित करेगी कि आत्मा समय से सीमित नहीं है, क्योंकि यह शाश्वत है, बिना किसी शुरुआत के। चूंकि आत्मा अतीत और भविष्य में एक ही है, इसलिए यह समय के अधीन नहीं है।
संदेह:- पदार्थ से क्या अभिप्राय है?
स्पष्टीकरण:- पदार्थ वह है जिसमें तीन प्रकार के भेद होते हैं, अर्थात्, (i) समान जाति में भेद जिसे सजातीय भेद कहा जाता है, (ii) विभिन्न जातियों में भेद जिसे विजातीय भेद कहा जाता है, और (iii) एक ही वस्तु में आंतरिक भेद जिसे स्वगत भेद कहा जाता है। उदाहरण के लिए, दो वृक्षों के बीच का अंतर सजातीय भेद है; एक वृक्ष और एक पत्थर के बीच का अंतर विजातीय भेद है; और एक वृक्ष के विभिन्न भागों जैसे कि पत्तियाँ, फूल, फल आदि के बीच का अंतर स्वगत भेद है। चूँकि आत्मा में इन तीन प्रकार के भेद नहीं होते, इसलिए यह पदार्थ से सीमित नहीं होती।
संदेह:- ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त तीन प्रकार के भेद आत्मा में अनुपस्थित नहीं हैं, क्योंकि एक ही चेतना ब्रह्म (परम आत्मा), ईश्वर (सर्वव्यापी आत्मा), कूटस्थ (आधारभूत आत्मा), और जीव (व्यक्तिगत आत्मा) के रूप में प्रकट होती है। इसलिए, यहाँ सजातीय भेद प्रतीत होता है। ब्रह्म (आत्मा) और अनात्मा (संसार) जैसे पूरी तरह असमान तत्वों के अस्तित्व के कारण विजातीय भेद प्रतीत होता है। साथ ही, ब्रह्म में सत, चित और आनंद जैसे तीन भिन्न गुण होने के कारण स्वगत भेद भी प्रतीत होता है। अतः जब आत्मा में ये भेद स्पष्ट रूप से दिखते हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि इनमें कोई भेद नहीं है?
स्पष्टीकरण:- जब इन भेदों को सही तरीके से समझा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे केवल आभासी हैं। उदाहरण के लिए, आकाश वास्तव में एक ही है, फिर भी यह विभिन्न सीमाओं के कारण सार्वभौमिक आकाश, बादलों का आकाश, घड़े का आकाश, जल में परावर्तित आकाश आदि के रूप में दिखता है। इसी प्रकार, एक ही चेतना माया की सीमाओं के कारण ब्रह्म और ईश्वर के रूप में, और अविद्या की सीमाओं के कारण कूटस्थ और जीव के रूप में प्रकट होती है। इसलिए, जब हम गहराई से जांच करते हैं, तो पाते हैं कि आत्मा में कोई सजातीय भेद नहीं है।
अब हम आत्मा में विजातीय भेद की अनुपस्थिति को समझाएँगे। बिना रस्सी के, सांप का आरोपण नहीं हो सकता; बिना आकाश के उसमें नीलिमा की प्रतीति नहीं हो सकती। इसी प्रकार, बिना आत्मा के, अनात्मा (संसार) का अस्तित्व नहीं हो सकता। संक्षेप में, बिना आधार के, सभी आरोपण वास्तव में अवास्तविक होते हैं। अवास्तविकता का अर्थ यह है कि कोई वस्तु तीनों कालों (भूत, वर्तमान, भविष्य) में अस्तित्वहीन होती है, जैसे कि बाँझ स्त्री का पुत्र या खरगोश के सींग। इस प्रकार, अनात्मा का दृष्टिकोण अद्वैत वेदांत के अनुसार अवास्तविक होने के कारण, विजातीय भेद आत्मा में नहीं हो सकता।
अंत में, आत्मा में स्वगत भेद की अनुपस्थिति को समझते हैं। चूँकि आत्मा गुणों और भागों से रहित है, इसलिए आत्मा को दर्शाने के लिए 'आत्मा', 'साक्षी', 'कूटस्थ', 'परमार्थिक', 'प्रज्ञा', 'ब्रह्म', 'सत्', 'चित्', 'आनंद', 'नित्य', 'एकः', 'परिपूर्ण' आदि सकारात्मक शब्दों तथा 'अस्थूल', 'अनणु', 'अद्वैत', 'अचिंत्य', 'अविकारी', 'अविनाशी', 'अकर्ता', 'अकारयिता' आदि नकारात्मक शब्दों का उपयोग केवल आत्मा को इंगित करने के लिए किया जाता है। ये किसी भी प्रकार से आत्मा के आंतरिक भेद को सूचित नहीं करते, क्योंकि आत्मा अविभाज्य और अपरिवर्तनशील है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आत्मा में स्वगत भेद भी नहीं है।
संदेह:- 'हस्त', 'कर' और 'पाणि' जैसे शब्द एक ही वस्तु, अर्थात् हाथ, को दर्शाते हैं और परस्पर विनिमेय हैं। लेकिन 'सत्', 'चित्' और 'आनंद' तीन भिन्न चीजों को दर्शाते प्रतीत होते हैं, जैसे वृक्ष के पत्ते, फल आदि, जो वृक्ष से भिन्न होते हैं। इसलिए, ऐसा लगता है कि आत्मा, जिसे इन तीन शब्दों द्वारा इंगित किया गया है, स्वगत भेद से युक्त होनी चाहिए। कृपया इसे स्पष्ट करें।
स्पष्टीकरण:- नहीं। वास्तव में, इन तीन शब्दों द्वारा कोई आंतरिक भेद संकेतित नहीं किया जाता। यह अभिव्यक्ति 'प्रकाश लाल-गर्म-तेजस्वी है' जैसी है, जिसमें तीनों शब्द उसी प्रकाश को इंगित करते हैं और प्रकाश के आंतरिक भेद को नहीं दर्शाते। इसी प्रकार, आत्मा में भी स्वगत भेद नहीं है।
संदेह:- फिर श्रुति बार-बार क्यों सिखाती है कि आत्मा सत्, चित् और आनंद से युक्त है? क्या आत्मा को केवल एक गुण से नहीं पहचाना जा सकता?
स्पष्टीकरण:- कृपया सुनें कि श्रुति के इन कथनों का तात्पर्य क्या है। अज्ञान के कारण लोग इस स्थूल ब्रह्मांड को 'सत्' (वास्तविकता), इस जड़ बुद्धि को 'चित्' (चेतना), और पत्नी, पुत्र आदि के सुख को 'आनंद' मान लेते हैं। इस प्रकार वे आत्मा के सत्-चित्-आनंद को इस असत्य जगत, जड़ बुद्धि और नश्वर भौतिक सुखों के रूप में देखते हैं, जो वास्तव में अस्थायी, जड़ और पीड़ादायक होते हैं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए, श्रुति व्यक्ति को उनकी वास्तविक प्रकृति का ज्ञान कराती है।
श्रुति कहती है: "हे जीव! यह समझने के लिए कि तुम स्वयं सत्-चित्-आनंद हो, मैं कहती हूँ कि आत्मा सत् है, असत् (अवास्तविक) नहीं; आत्मा चित् है, जड़ (अचेतन) नहीं; और आत्मा आनंद है, दुःख नहीं।" इस प्रकार, श्रुतियाँ लोगों को उनकी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को सिखाने के लिए इन तीनों शब्दों का उपयोग करती हैं, न कि आत्मा में किसी भेद को इंगित करने के लिए।
संदेह:- हे स्वामी! हम कैसे समझ सकते हैं कि यह अविभाज्य स्वरूप ही श्रुति का वास्तविक अभिप्राय है?
स्पष्टीकरण:- सभी श्रुतियों का उद्देश्य केवल आत्मा की अविभाज्य प्रकृति को स्पष्ट करना है। इसे हम षड्लिंग (छः प्रमाण) के माध्यम से समझ सकते हैं।
संदेह:- अब जब कि श्रुति के प्रमाण से सत्-चित्-आनंद की अविभाज्यता सिद्ध हो गई है, तो इसे तर्क (युक्ति) द्वारा कैसे सिद्ध किया जाए?
स्पष्टीकरण:- सत् या तो स्वयं प्रकाशित होना चाहिए या बाह्य साधनों से प्रकाशित किया जाना चाहिए। यदि यह स्वयं प्रकाशित है, तो सत् ही चित् है। यदि इसे बाहरी साधनों द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए, तो यह या तो सत् से पूर्णतः भिन्न होगा या दूसरा सत् होगा। यदि यह सत् से भिन्न है, तो यह असत् होगा, जो कि असंभव है। इसलिए, सत् स्वयं प्रकाशित होता है और इसलिए यह चित् भी है।
अब इस आत्म-प्रकाशमान सत् को आनंद रूप में सिद्ध किया जाता है। चूँकि अस्तित्व अद्वैत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यह स्वयं ही आनंद है। सीमित वस्तुओं में पूर्णता नहीं होती। पूर्ण-असीम-अस्तित्व ही आनंद है।
इस प्रकार, यह तर्क और अनुभव द्वारा भी सिद्ध हो जाता है कि सत्, चित् और आनंद समानार्थी हैं और वे एक अविभाज्य सत्ता, आत्मा, को इंगित करते हैं।
उपसंहार
आत्मा पूर्ण आनंद स्वरूप है। पीड़ा बाह्य और कारणजन्य है। यह शरीरधारण के कारण उत्पन्न होती है और शरीरधारण कर्म के कारण होता है। कर्म राग और द्वेष से उत्पन्न होता है, जो अहंकार से जन्म लेते हैं। अहंकार अविवेक के कारण उत्पन्न होता है, और अविवेक अज्ञान का परिणाम है। उस अज्ञान का नाश ज्ञान द्वारा किया जाना चाहिए। ज्ञान विचार से उत्पन्न होता है। इसलिए, व्यक्ति को इस प्रकार सत्य का अन्वेषण करना चाहिए: "आत्मा सत्-चित्-आनंद-स्वरूप है। यह जगत असत्य, जड़ और दुःखमय है और यह केवल एक आरोपण मात्र है।"
इस प्रकार का विचार, जब महावाक्य "तत् त्वम् असि" के गहन विश्लेषण से उत्पन्न ज्ञान के साथ किया जाता है, तो यह एक दृढ़ आंतरिक विश्वास उत्पन्न करता है, जो यह अप्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है कि "मैं ब्रह्म हूँ।" जब इस ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा समझ लिया जाता है, तो अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यह स्थिति परमहंस संन्यासी की अवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसे बहुदक, कुटीचक और हंस संन्यासियों की तुलना में अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए। भगवान शंकराचार्य के अनुसार, चाहे वह व्यक्ति ब्राह्मण हो या चांडाल, यदि वह इस ज्ञान में स्थिर हो जाता है, तो वह स्वयं परमगुरु के समान होता है।
अतः व्यक्ति को श्रवण, मनन और ध्यान के मार्ग को अपनाना चाहिए, जैसा कि पहले वर्णित किया गया है, और परम अद्वैत ब्रह्म में स्थिर हो जाना चाहिए, जो परम आनंद, शाश्वत, शुद्ध और सदा मुक्त है। आचार्य को सिखाने के लिए और शिष्य को सीखने के लिए और क्या बचा है? अब सिखाने या सीखने के लिए कुछ भी शेष नहीं है।
ॐ तत् सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।
परिशिष्ट I वेदांत बोध (श्री स्वामी शिवानंद)
1. प्रश्न:
उपाधि का क्या अर्थ है?
उत्तर: उपाधि का अर्थ है
सीमित करने वाला उपकरण या
स्थिति।
2. प्रश्न:
एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर: घड़ा एक उपाधि है
जो "घटाकाश"
या घड़े में स्थित आकाश
शब्द को जन्म देती है।
यह घड़ा ही सार्वभौमिक आकाश
को सीमित करता है। इसी
प्रकार, भौतिक शरीर,
जो अविद्या का परिणाम है,
एक उपाधि है जिसने ब्रह्म
को जीव के रूप में
सीमित कर दिया है, जबकि वास्तव में जीव
ब्रह्म के समान है। मन
भी अविद्या का एक अन्य
उपाधि है। जब घड़ा टूट
जाता है, तो घटाकाश सार्वभौमिक आकाश में
विलीन हो जाता है। इसी
प्रकार, जब जीवन्मुक्त का भौतिक शरीर नष्ट
हो जाता है,
तो वह विदेहमुक्ति प्राप्त करता है।
3. प्रश्न:
उपहित चैतन्य क्या है?
उत्तर: उपहित चैतन्य वह चैतन्य
(बुद्धि) है जो उपाधि से
संबंधित होती है। जहाँ भी
उपाधि होती है,
वहाँ उपहित चैतन्य होता है।
मन एक उपाधि है। मन
से जुड़ी चेतना को ही
मन का उपहित चैतन्य कहते
हैं।
4. प्रश्न:
जीव की उपाधि क्या है?
उत्तर: अविद्या (अज्ञान)।
5. प्रश्न:
ईश्वर की उपाधि क्या है?
उत्तर: माया।
6. प्रश्न:
मन के धर्म
(गुण) क्या हैं?
उत्तर: राग और द्वेष (आकर्षण और विकर्षण, पसंद और नापसंद, प्रेम और घृणा), सुख और दुःख (आनंद और पीड़ा) मन के धर्म हैं।
7. प्रश्न:
माया और अविद्या में क्या अंतर है?
उत्तर: माया शुद्ध सत्व है,
जबकि अविद्या अशुद्ध या मलिन
सत्व (राजस और तामस से
मिश्रित सत्व) है।
8. प्रश्न:
मोक्ष का स्वरूप क्या है?
उत्तर: समस्त दुःखों का नाश
और परम आनंद की प्राप्ति ही मोक्ष
का स्वरूप है।
9. प्रश्न:
सर्व-दुःख-निवृत्ति क्या है?
उत्तर: अविद्या और इसके प्रभावों
(जन्म, मृत्यु आदि)
का नाश।
10. प्रश्न:
परम-आनंद-प्राप्ति क्या है?
उत्तर: नित्य, निरुपाधिक, निरतिशय आनंद
(शाश्वत, असीम और अनंत आनंद)
की प्राप्ति।
11. प्रश्न:
मोक्ष का हेतु
(कारण) क्या है?
उत्तर: दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म-ज्ञान
(स्थायी, प्रत्यक्ष आत्मसाक्षात्कार)।
12. प्रश्न:
दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म-ज्ञान क्या है?
उत्तर: यह भावना-रहित ब्रह्म-ज्ञान है।
13. प्रश्न:
भावना-रहित का क्या अर्थ
है?
उत्तर: यह तीन प्रकार की
भावनाओं से मुक्ति है: (i) संशय-भावना
(संदेह), (ii) असंभावना
(असंभवता), और (iii) विपरीत-भावना
(गलत धारणा)।
14. प्रश्न:
अधृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म-ज्ञान क्या है?
उत्तर: यह भावना-सहित ज्ञान (तीनों भावनाओं से युक्त ज्ञान) है।
15. प्रश्न:
दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म-ज्ञान कैसे प्राप्त
किया जा सकता है?
उत्तर: निरंतर ब्रह्म-विचार
(ब्रह्म पर चिंतन)
के माध्यम से।
16. प्रश्न:
कृपा के चार प्रकार कौन
से हैं?
उत्तर: ईश्वर-कृपा,
गुरु-कृपा, शास्त्र-कृपा और आत्म-कृपा।
17. प्रश्न:
जीव का स्वरूप क्या है?
उत्तर: कूटस्थ + अविद्या
+ आभास चैतन्य (अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य)।
18. प्रश्न:
ईश्वर का स्वरूप क्या है?
उत्तर: ब्रह्म + माया
+ माया में प्रतिबिंबित चैतन्य।
19. प्रश्न:
माया का स्वरूप क्या है?
उत्तर: माया सत् और असत्
दोनों से भिन्न,
अनादि, भावरूप और अनिर्वचनीय है।
यह न तो ब्रह्म के
समान सत् है और न
ही खरगोश के सींग या
आकाश में कमल की तरह
असत् है। यह अनादि है
और केवल ब्रह्म-ज्ञान से समाप्त
होती है। ब्रह्म अनादि और
अनंत है।
20. प्रश्न:
विराट कौन है?
उत्तर: वह भौतिक जगत का
आत्मा है। वह संपूर्ण स्थूल
शरीरों और भौतिक वस्तुओं में
प्रतिबिंबित चैतन्य
है। वैश्वानर विराट का ही
एक अन्य नाम है।
21. प्रश्न:
हिरण्यगर्भ कौन है?
उत्तर: वह सूक्ष्म जगत का आत्मा है।
वह संपूर्ण लिंग-शरीरों में प्रतिबिंबित चैतन्य है।
इसे 'स्वर्ण-अंड'
भी कहा जाता है। सूत्रात्मा उसका एक
अन्य नाम है।
22. प्रश्न:
ईश्वर कौन है?
उत्तर: वह कारण जगत का
आत्मा है। वह संपूर्ण कारण
शरीरों में प्रतिबिंबित चैतन्य है। उसका एक
अन्य नाम अव्याकृत है।
23. प्रश्न:
व्यष्टि क्या है?
उत्तर: इसका अर्थ है एकल
या व्यक्तिगत (पिंड)। एक घर,
एक वृक्ष या एक माचिस
की तीली व्यष्टि है।
24. प्रश्न:
समष्टि क्या है?
उत्तर: इसका अर्थ है 'समूह', 'संग्रह',
'संपूर्ण ब्रह्मांड'। एक गाँव,
एक वन या माचिस का
डिब्बा समष्टि है।
25. प्रश्न: विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर को एक अन्य प्रकार से परिभाषित करें।
उत्तर:
● विराट: संपूर्ण स्थूल शरीरों, वस्तुओं आदि का योगफल + प्रतिबिंबित चैतन्य।
● हिरण्यगर्भ: संपूर्ण सूक्ष्म शरीरों का योगफल + प्रतिबिंबित चैतन्य।
● ईश्वर: संपूर्ण कारण शरीरों का योगफल + प्रतिबिंबित चैतन्य।
26. प्रश्न:
विश्व (Visva) क्या
है?
उत्तर: वह जाग्रत अवस्था में
स्थित जीव है। वह जाग्रत
चेतना में रहने वाला जीव
है। वह व्यष्टि
(व्यक्तिगत) है। वह स्थूल शरीर
का अधिकारी है। वह व्यावहारिक जीव (सूक्ष्म ब्रह्मांड) है। वह
चैतन्य है जो जाग्रत अवस्था
में व्यक्तिगत स्थूल शरीर में
प्रतिबिंबित होता
है। विश्व जाग्रत चेतना का
जीव है।
27. प्रश्न:
तैजस (Taijasa) क्या
है?
उत्तर: वह प्रातिभासिक जीव है। वह स्वप्न
चेतना का जीव है। वह
व्यष्टि-सूक्ष्म-शरीर-अभिमानी है। जो चैतन्य लिंग-शरीर में प्रतिबिंबित होता है,
वही तैजस कहलाता है।
28. प्रश्न:
प्राज्ञ (Prajna) क्या
है?
उत्तर: प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था में स्थित जीव
है। वह कारण शरीर का
अभिमानी है। जो चैतन्य कारण
शरीर से जुड़ा होता है,
वही प्राज्ञ कहलाता है।
29. प्रश्न:
कूटस्थ (Kutastha) क्या
है?
उत्तर: वह जीव का अधिष्ठान
(आधार) या सहारा है। वह
मन में उत्पन्न होने वाले विकारों और
तीन अवस्थाओं (जाग्रत,
स्वप्न और सुषुप्ति) का मूक
साक्षी है।
30. प्रश्न:
कूटस्थ का क्या अर्थ है?
उत्तर: कूटस्थ का अर्थ है
अपरिवर्तनशील या
चट्टान के समान दृढ़।
31. प्रश्न:
इसे कूटस्थ क्यों कहा जाता
है?
उत्तर: जैसे लोहार की धौंकनी
में स्थित धातु अपरिवर्तनशील रहती
है, लेकिन वह लोहे के
टुकड़ों को विभिन्न रूपों में ढाल देती
है, वैसे ही कूटस्थ ब्रह्म
अपरिवर्तनशील रहता
है, जबकि शरीर और मन
अनेक प्रकार के परिवर्तन से
गुजरते हैं।
32. प्रश्न:
क्या कूटस्थ ब्रह्म ब्रह्म से
भिन्न है?
उत्तर: नहीं, कूटस्थ ब्रह्म और
ब्रह्म एक ही हैं।
33. प्रश्न:
कूटस्थ के अन्य नाम क्या
हैं?
उत्तर: प्रत्यगात्मा, क्षेत्रज्ञ, अंतर्यामी, कूटस्थ चैतन्य,
कूटस्थ ब्रह्म, साक्षी,
दृष्टा, उपद्रष्टा, तुरीय आदि।
34. प्रश्न:
साक्षी (कूटस्थ) के अस्तित्व को
कैसे सिद्ध करेंगे?
उत्तर: जैसे कोई वृक्ष को
देखता है, वैसे ही कोई
तो होना चाहिए जो मन
या बुद्धि की गतिविधियों का
साक्षी बने। एक गिलास स्वयं
को नहीं देख सकता। केवल
जीव ही अपनी दृष्टि इंद्रिय
की सहायता से गिलास को
देख सकता है। यदि यह
कहा जाए कि गिलास स्वयं
को देख सकता है, तो यह तर्कहीन होगा।
इसलिए, वही कूटस्थ है जो
मन में उत्पन्न होने वाले विकारों का
साक्षी है।
35. प्रश्न:
अध्यास (Adhyasa) का
क्या अर्थ है?
उत्तर: अध्यास का अर्थ है
आरोपण। जब किसी वस्तु के
गुणों को गलत तरीके से
किसी अन्य वस्तु पर आरोपित
कर दिया जाता है, तो उसे अध्यास कहते
हैं।
36. प्रश्न:
एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर: जैसे सीप को चांदी
समझ लिया जाता है। इसमें
चांदी का अध्यास सीप पर
कर दिया गया है। इसी
प्रकार, शरीर जड़
(अचेतन) होता है,
लेकिन यह चेतन प्रतीत होता
है क्योंकि आत्मा के गुण
बुद्धि और शरीर पर आरोपित
हो जाते हैं।
37. प्रश्न:
अध्यारोप (Adhyaropa) क्या
है?
उत्तर: यह अध्यास के समान
है। अध्यारोप और अध्यास समानार्थी शब्द हैं।
संसार और शरीर ब्रह्म पर
अध्यारोपित हैं।
38. प्रश्न:
अपवाद (Apavada) क्या
है?
उत्तर: इसका अर्थ है निषेध
या किसी गलत आरोपण को
हटाना। जैसे सांप की भ्रांति
रस्सी पर होती है और
जब ज्ञान होता है, तो केवल रस्सी का
ही अस्तित्व रह जाता है,
वैसे ही ब्रह्म पर आरोपित
संसार को झूठा समझकर केवल
ब्रह्म को ही सत्य माना
जाता है।
39. प्रश्न:
किसी वस्तु के पाँच भाग
कौन से हैं?
उत्तर: नाम (Nama), रूप
(Rupa), अस्ति (Asti), भाति
(Bhati), और प्रिया
(Priya)।
40. प्रश्न:
नाम-रूप (Nama-Rupa) क्या है?
उत्तर: नाम और रूप जगत
में दुःख का कारण हैं,
विशेषकर अविवेकी (विचारहीन) व्यक्तियों के
लिए।
41. प्रश्न:
अस्ति, भाति, प्रिया क्या हैं?
उत्तर: ये सत्-चित्-आनंद के प्रतीक
हैं। ये विवेकी व्यक्तियों के
लिए सुख-प्राप्ति और दुःख-निवृत्ति के कारण होते हैं।
अस्ति सत् है,
भाति चित् है,
और प्रिया आनंद है।
42. प्रश्न:
सूर्य के जल में प्रतिबिंब और ब्रह्म
के अविद्या में प्रतिबिंब की
तुलना करें।
उत्तर: जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के
फैलने से बढ़ता है, सिकुड़ने से छोटा होता
है, हिलने से काँपता है,
और विभाजन से विभाजित हो
जाता है, वैसे ही ब्रह्म,
जो वास्तव में अखंड और
अपरिवर्तनशील है,
उपाधियों (शरीर, मन)
के अनुसार बदलता प्रतीत होता
है।
43. प्रश्न:
'तत् त्वम् असि'
महावाक्य किस उपनिषद में मिलता
है?
उत्तर: सामवेद के छांदोग्य उपनिषद
में।
44. प्रश्न:
महावाक्य (Mahavakya) क्या
है?
उत्तर: महावाक्य का अर्थ है
महान वचन या दिव्य उपदेश।
45. प्रश्न:
'तत् त्वम् असि'
किस प्रकार का वाक्य है?
उत्तर: यह उपदेश वाक्य है,
जिसे गुरु शिष्य को कहता
है।
46. प्रश्न:
वाच्यार्थ (Vachyartha) क्या
है?
उत्तर: यह किसी शब्द का
शब्दार्थ या प्रत्यक्ष अर्थ होता है।
47. प्रश्न:
लक्ष्यार्थ (Lakshyartha) क्या
है?
उत्तर: यह किसी शब्द का
संकेतार्थ या गूढ़ अर्थ होता
है।
48. प्रश्न:
'तत्' पद का वाच्यार्थ क्या
है?
उत्तर: ईश्वर।
49. प्रश्न:
'तत्' पद का लक्ष्यार्थ क्या
है?
उत्तर: ब्रह्म।
50. प्रश्न:
'त्वम्' पद का वाच्यार्थ क्या
है?
उत्तर: जीव।
51. प्रश्न:
'त्वम्' पद का लक्ष्यार्थ क्या
है?
उत्तर: कूटस्थ।
52. प्रश्न:
'तत् त्वम् असि'
महावाक्य में जीव और ब्रह्म
की एकता को कैसे समझाया
जा सकता है?
उत्तर: उदाहरण के लिए, 'सोयम देवदत्तः' का प्रसिद्ध दृष्टांत लें।
आपने जनवरी 1928 में वृंदावन में
देवदत्त को साधारण पोशाक में
बाजार में चलते हुए देखा।
फिर 1931 में
बनारस में आपने उसे वर्दी
और टोपी पहने कार में
घूमते देखा। आपने अब उसे
देवदत्त के रूप में पहचाना,
कपड़ों, समय और स्थान को
नकारते हुए। आपने केवल व्यक्ति
देवदत्त की पहचान की, बाकी वस्तुओं को छोड़ दिया।
इसी प्रकार, जब हम जीव
के संदर्भ में अविद्या और
उसके प्रभावों को,
जीव में प्रतिबिंबित आभास चैतन्य और जीव
के मिथ्या धर्मों को हटा
देते हैं, और ईश्वर के
संदर्भ में माया और उसके
प्रभावों को, माया में प्रतिबिंबित चैतन्य और
ईश्वर के गुणों को हटा
देते हैं, तब केवल केवला
शुद्ध चैतन्य शेष रहता है,
जो ईश्वर और जीव दोनों
के लिए आधार है। ईश्वर
और जीव की स्वरूप-लक्षण (सत्-चित्-आनंद स्वरूप) एक ही होती हैं।
अंतर केवल तटस्थ-लक्षण में है,
जो मिथ्या या आरोपित है।
53. प्रश्न:
'पदार्थ शोधन' (Padartha
Sodhana) क्या है?
उत्तर: जैसे घटाकाश और महाकाश
की एकता को कल्पित उपाधि
को नकार कर देखा जाता
है, जैसे जलाकाश और मेघाकाश
की एकता को केवल उनके
आधार को देखकर समझा जाता
है, वैसे ही
'तत् त्वम् असि'
महावाक्य में जीव और ईश्वर
के कल्पित उपाधियों (तत् और
त्वम् पद के वाच्यार्थ) को हटाकर कूटस्थ और
ब्रह्म की एकता को देखना
ही पदार्थ-शोधन है।
54. प्रश्न:
जीव और ब्रह्म की एकता
को दर्शाने वाली लक्षणा क्या
है?
उत्तर: भाग-त्याग लक्षणा (Bhaga-Tyaga Lakshana) या जहद-अजहल्लक्षणा।
55. प्रश्न:
भाग-त्याग का क्या अर्थ
है?
उत्तर: इसमें कुछ
(जैसे उपाधि) को त्याग कर
केवल चैतन्य को स्वीकार किया
जाता है। मिथ्या उपाधियों को
नकारकर केवल शुद्ध चैतन्य या
शुद्ध ब्रह्म को स्वीकार करना
ही भाग-त्याग है।
56. प्रश्न:
माया की दो प्रमुख शक्तियाँ कौन-सी हैं?
उत्तर: आवरण शक्ति
(Avarana Sakti) और विक्षेप
शक्ति (Vikshepa Sakti)।
57. प्रश्न:
आवरण शक्ति क्या करती है?
उत्तर: यह जीव को ढक
देती है और उसे उसके
वास्तविक सत्-चित्-आनंद स्वरूप को
जानने से रोकती है। यह
जीव को उसके तीन शरीरों
और पंचकोशों से अलग पहचानने
से भी रोकती है।
58. प्रश्न:
विक्षेप शक्ति क्या करती है?
उत्तर: यह जीव को उसके
स्थूल शरीर से तादात्म्य कराती
है और संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रक्षिप्त करती
है।
59. प्रश्न:
सजातीय भेद (Sajatiya Bheda) क्या है?
उत्तर: जब एक ही जाति
(प्रकार) के दो सदस्यों में
भेद होता है,
जैसे एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, या एक अंग्रेज और
एक भारतीय।
60. प्रश्न:
विजातीय भेद (Vijatiya Bheda) क्या है?
उत्तर: जब दो भिन्न प्रकार
की वस्तुओं में भेद हो,
जैसे मनुष्य और गाय, या वृक्ष और पत्थर।
61. प्रश्न:
स्वगत भेद (Svagata Bheda) क्या है?
उत्तर: जब एक ही वस्तु
के आंतरिक भागों में भेद
हो, जैसे जल में लहरें
और भंवर, मनुष्य में हाथ,
पैर, सिर आदि,
या वृक्ष में फल, फूल, टहनी और पत्तियाँ।
62. प्रश्न:
क्या ब्रह्म में सजातीय भेद
है?
उत्तर: नहीं।
63. प्रश्न:
क्यों?
उत्तर: ब्रह्म अनंत
(Aparicchinna, Ananta, Bhuma) है। अनंत
केवल एक हो सकता है।
दो अनंत नहीं हो सकते।
इसलिए, ब्रह्म केवल एक अद्वितीय सत्ता है।
'एकमेव अद्वितीयम्' यही श्रुति का
प्रमाण है।
64. प्रश्न:
क्या ब्रह्म में विजातीय भेद
है, क्योंकि यह संसार से
भिन्न प्रतीत होता है?
उत्तर: नहीं।
65. प्रश्न:
क्यों?
उत्तर: ब्रह्म ही निमित्त और
उपादान कारण दोनों है। इसलिए
संसार ब्रह्म से भिन्न नहीं
हो सकता। जो ब्रह्मांड के
रूप में प्रकट होता है,
वह ब्रह्म ही है। श्रुति
कहती है: 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'
- "यह सब ब्रह्म ही है।"
जैसे बाँझ स्त्री का काल्पनिक पुत्र उसे
माता नहीं बना सकता, वैसे ही यह मिथ्या
ब्रह्मांड ब्रह्म में द्वैत नहीं
ला सकता।
66. प्रश्न:
क्या ब्रह्म में स्वगत भेद
है?
उत्तर: नहीं।
67. प्रश्न:
क्यों?
उत्तर: सत्, चित् और आनंद
तीन अलग-अलग नहीं हैं,
बल्कि वे ब्रह्म का स्वरूप
हैं। यह केवल शब्द भेद
है, जैसे हस्त,
कर और पाणि
(तीनों हाथ के लिए प्रयुक्त होते हैं)। सत् ही
चित् है, चित् ही सत्
है, चित् ही आनंद है,
और सत् ही आनंद है।
जैसे अग्नि में ताप, प्रकाश और लालिमा स्वाभाविक गुण हैं,
वैसे ही सत्-चित्-आनंद ब्रह्म का
स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म
में स्वगत भेद नहीं है।
68. प्रश्न:
मन में मलों
(काम, क्रोध आदि)
के अस्तित्व को कैसे जाना
जा सकता है?
उत्तर: जैसे धुएँ से अग्नि
के होने का अनुमान लगाया
जाता है, वैसे ही यदि
मन में अशुभ वासनाएँ, इंद्रिय भोग की इच्छाएँ
और निषिद्ध कर्मों की प्रवृत्ति उत्पन्न हो,
तो यह मन में मलों
की उपस्थिति का संकेत है।
69. प्रश्न:
चित्त में विक्षेप की उपस्थिति को कैसे जाना जाए?
उत्तर: जब मन वेदांतिक श्रवण
या स्वरूप में स्थिर नहीं
हो पाता और बाह्य वस्तुओं
की ओर भागता है, तो यह चित्त में
विक्षेप का संकेत है।
70. प्रश्न:
आवरण क्या है?
उत्तर: यह अज्ञान का आवरण
है जो आत्मा को ढक
लेता है, जैसे बादल सूर्य
को छिपा देते हैं और
हरी काई जल को ढक
लेती है।
71. प्रश्न:
आवरण की उपस्थिति को कैसे जाना जाए?
उत्तर: जब व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता
है, ब्रह्म के प्रत्यक्ष ज्ञान
से वंचित रहता है, और 'मैं ब्राह्मण हूँ',
'मैं धनी हूँ',
'मैं निर्धन हूँ',
'मैं गृहस्थ हूँ',
जैसी धारणाएँ रखता है, तो यह चित्त में
आवरण दोष का संकेत है।
72. प्रश्न:
आवरण को कैसे हटाया जा
सकता है?
उत्तर: जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर
हो जाता है,
वैसे ही ब्रह्म के प्रत्यक्ष ज्ञान से
आवरण समाप्त हो जाता है।
73. प्रश्न:
ब्रह्म की तटस्थ लक्षणा (Tatastha Lakshana) क्या
है?
उत्तर: सगुण ब्रह्म को तटस्थ
लक्षणा के रूप में समझा
जाता है। ब्रह्म सृष्टि, पालन और संहार का
कारण है—इस परिभाषा से
ब्रह्म की केवल अप्रत्यक्ष धारणा
होती है।
74. प्रश्न:
ब्रह्म की स्वरूप लक्षणा (Svarupa Lakshana) क्या
है?
उत्तर: सत्-चित्-आनंद। यह ब्रह्म
की वास्तविक और मौलिक परिभाषा
है।
75. प्रश्न:
अतद्व्यावृत्ति लक्षणा
(Atadvyavritti Lakshana) क्या है?
उत्तर: यह आत्मा को इंगित
करती है, जो नेति-नेति सिद्धांत के माध्यम से देह
आदि अनात्म वस्तुओं को नकारने के बाद
शेष बचती है।
76. प्रश्न:
जहल्लक्षणा (Jahallakshana) क्या
है? उदाहरण दीजिए।
उत्तर: 'गंगायां घोषः'—इसका अर्थ होता
है कि गंगा में शोरगुल
है। वास्तव में,
इसका तात्पर्य गंगा के तट
पर स्थित गाँव के लोगों
के शोरगुल से है। यहाँ
'गंगा' को छोड़कर
'तट' को ग्रहण किया गया
है।
77. प्रश्न:
अजहाल्लक्षणा (Ajahallakshana) का
उदाहरण दीजिए।
उत्तर: 'श्वेतो धावति'—इसका अर्थ है
'श्वेत दौड़ रहा है'। इसका तात्पर्य 'श्वेत अश्व दौड़ रहा
है' से है। यहाँ 'अश्व' शब्द जोड़ा गया
है।
78. प्रश्न:
नेति-नेति सिद्धांत को किसी कहानी से
समझाइए।
उत्तर: एक आठ वर्षीय बालक
बाजार में रो रहा था
क्योंकि उसका पिता खो गया
था। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, 'क्या यह लंबा गोरा
आदमी तुम्हारा पिता है?' बालक बोला,
'नहीं।' फिर उस व्यक्ति ने
पूछा, 'क्या यह फूलों की
टोकरी लिए हुए आदमी तुम्हारा पिता है?'
बालक ने फिर मना कर
दिया। इस प्रकार,
जब तक सही विशेषताओं वाला
व्यक्ति नहीं मिल जाता, तब तक अन्य सभी
को नकारा जाता है। इसी
प्रकार, जब कोई ब्रह्म की
खोज करता है,
तो वह देखता है कि
घड़ा ब्रह्म नहीं है, पत्थर ब्रह्म नहीं है,
वृक्ष ब्रह्म नहीं है, शरीर ब्रह्म नहीं है।
अंततः जो शुद्ध सत्ता बचती
है, वही ब्रह्म है।
79. प्रश्न:
साधना के परिणामस्वरूप बुद्धि में क्या परिवर्तन होता है?
कोई उदाहरण दीजिए।
उत्तर: आत्मा का प्रतिबिंब प्राप्त
करने के लिए एक उपयुक्त
आधार (बुद्धि) की आवश्यकता होती
है। यदि ऐसा आधार न
हो, तो आत्मा स्वयं को
प्रतिबिंबित नहीं
कर सकती।
उदाहरण के लिए,
यदि एक दर्पण ठीक से
सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता
है, तो सूर्य की छवि
उसमें स्पष्ट दिखेगी। यदि दर्पण टूट जाए
या चूर्ण हो जाए, तो प्रतिबिंब नष्ट हो जाएगा। इसी
प्रकार, जब बुद्धि
(जो आत्मा के प्रतिबिंब का
आधार है) विचारशून्यता और विवेक द्वारा नष्ट
हो जाती है,
तब आत्मा का प्रतिबिंब भी
लुप्त हो जाता है और
जीवभाव समाप्त होकर मोक्ष प्राप्त
होता है।
80. प्रश्न:
अवांतर वाक्य (Avantara
Vakya) क्या है?
उत्तर: यह स्वरूप बोध वाक्य
है, जैसे 'सत्-चित्-आनंद',
'सत्यम् ज्ञानम् अनंतम् ब्रह्म'।
81. प्रश्न:
महावाक्य (Mahavakya) क्या
है?
उत्तर: यह अभेद बोध वाक्य
है, जैसे 'अहं ब्रह्मास्मि', 'तत् त्वम् असि'।
82. प्रश्न:
वृत्ति व्यापत्ति (Vritti
Vyapti) क्या है?
उत्तर: मन की एक किरण
नेत्रों के माध्यम से बाहर
जाकर किसी वस्तु के आकार
को ग्रहण करती है और
उस वस्तु पर स्थित तूल
अविद्या (अज्ञान के आवरण) को हटा देती है।
यह वृत्ति व्यापत्ति है। वृत्ति का कार्य
किसी वस्तु के आवरण को
हटाना है।
83. प्रश्न:
फल व्यापत्ति (Phala
Vyapti) क्या है?
उत्तर: चैतन्य हमेशा वृत्ति के
साथ रहता है। वृत्ति किसी
वस्तु का आवरण हटाती है
और चैतन्य उसे प्रकाशित करता
है, जिससे वह वस्तु अनुभव
में आती है। उदाहरण: जब वृत्ति किसी घट
के आवरण को हटाती है
और चैतन्य उसे प्रकाशित करता
है, तब हम कहते हैं,
'यह घट है'।
84. प्रश्न:
अन्वय-व्यतिरेक
(Anvaya-Vyatireka) क्या है?
उत्तर: यह ज्ञानयोगी के आत्मनिष्ठ होने की एक प्रक्रिया है, जो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों होती है।अन्वय: जब कोई पंचकोशों में
आत्मा के अस्तित्व को देखता है। व्यतिरेक:
जब कोई देखता है कि
आत्मा पंचकोशों में नहीं है।
यह आत्मा को जानने का
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण है।
85. प्रश्न:
स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच संबंध
क्या है?
उत्तर: प्राण।
86. प्रश्न:
जाग्रत अवस्था में कितने शरीर
कार्य करते हैं?
उत्तर: तीन—स्थूल,
सूक्ष्म और कारण शरीर।
87. प्रश्न:
स्वप्न में कितने शरीर कार्य
करते हैं?
उत्तर: दो—सूक्ष्म और कारण शरीर।
88. प्रश्न:
सुषुप्ति में कितने शरीर कार्य
करते हैं?
उत्तर: केवल एक,
कारण शरीर।
89. प्रश्न:
कारण शरीर का अन्य नाम
क्या है?
उत्तर: आनंदमय कोश।
90. प्रश्न:
यह किससे बना है?
उत्तर: मूल अज्ञान।
91. प्रश्न:
ध्यान कौन करता है?
उत्तर: जीव।
92. प्रश्न:
ध्यान का लक्ष्य क्या है?
उत्तर: ब्रह्म।
93. प्रश्न:
ध्यान किस उपकरण के माध्यम
से किया जाता है?
उत्तर: मन।
94. प्रश्न:
समाधि में क्या होता है?
उत्तर: ध्यान समाप्त हो जाता
है। 'ओम', 'सोऽहं',
'अहं ब्रह्मास्मि' आदि का पुनरावृत्ति समाप्त हो
जाती है। जीव और ब्रह्म
एक हो जाते हैं।
95. प्रश्न:
दृष्टा (Drashta) का
क्या अर्थ है?
उत्तर: देखने वाला,
विषय।
96. प्रश्न:
दृश्य (Drisya) क्या
है?
उत्तर: देखी जाने वाली वस्तुएँ।
97. प्रश्न:
आत्मा ज्ञानेंद्रियों
से क्यों नहीं जानी जा
सकती?
उत्तर: यदि आत्मा ज्ञानेद्रियों से
जानी जा सके,
तो वह सीमित हो जाएगी।
लेकिन ब्रह्म अनंत है, इसलिए आत्मा इंद्रियों का
विषय नहीं बन सकती।
98. प्रश्न:
आत्मा को कैसे जाना जा
सकता है?
उत्तर: अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा।
99. प्रश्न:
ज्ञान के दो प्रकार कौन-कौन से हैं?
उत्तर: स्वरूप ज्ञान और वृत्ति
ज्ञान।
100.
प्रश्न: स्वरूप ज्ञान क्या है?
उत्तर: यह ब्रह्म का ज्ञान
है।
101.
प्रश्न: वृत्ति ज्ञान क्या है?
उत्तर: यह मानसिक वृत्ति (मन) के माध्यम से
वस्तुओं (विषयों) का ज्ञान है।
102.
प्रश्न: वेदांत के अनुसार सविकल्प
समाधि के कितने प्रकार हैं?
उत्तर: दृश्यानुविद्ध, दृश्याननुविद्ध, शब्दानुविद्ध और
शब्दाननुविद्ध।
103.
प्रश्न: निर्विकल्प समाधि के कितने
प्रकार होते हैं?
उत्तर: अद्वैत भावना रूप समाधि
(वृत्ति सहित) और अद्वैत अवस्था
रूप समाधि (वृत्ति रहित)।
104.
प्रश्न: संक्षेप में बंधन क्या
है?
उत्तर: 'देहोहं' (मैं शरीर हूँ)।
105.
प्रश्न: संक्षेप में मुक्ति क्या
है?
उत्तर: 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म
हूँ)।
106.
प्रश्न: अतद्वयावृत्ति
क्या है?
उत्तर: किसी वस्तु के विपरीत
चीज के माध्यम से सत्य
को जानने की प्रक्रिया। अर्थात
आत्मा तीन शरीरों से भिन्न
है और यह पंचकोशों से
भी अलग है।
107.
प्रश्न: कर्ता और भोक्ता कौन
है?
उत्तर: अंतःकरण। कूटस्थ अंतःकरण को
संचालित करता है और उसे
गति प्रदान करता है। अंतःकरण
सात्त्विक गुण प्रधान होता है,
किंतु इसमें रजोगुण भी होता
है। इसी रजोगुण के कारण
यह स्वतः क्रियाशील रहता है।
108.
प्रश्न: क्या अंतःकरण जड़ है या चेतन?
उत्तर: जड़। हालाँकि अंतःकरण जड़ है, फिर भी यह कूटस्थ
चैतन्य की उपस्थिति में चेतन के समान
प्रतीत होता है। जैसे लोहे
की छड़ चुम्बक के संपर्क
में आकर चुम्बक की भाँति
कार्य करने लगती है और
अन्य लोहे के टुकड़ों को
आकर्षित करती है।
109.
प्रश्न: परोक्ष ज्ञान क्या है?
उत्तर: यह ब्रह्म का अप्रत्यक्ष ज्ञान है,
जो ग्रंथों के अध्ययन से
प्राप्त होता है। यह ब्रह्म
की परोक्ष अवधारणा है, जो दूसरों पर
निर्भर होती है। परोक्ष का
अर्थ है किसी अन्य माध्यम
पर निर्भर होना। यह केवल
बौद्धिक स्तर पर ब्रह्म की
धारणा प्रदान करता है। इस
ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अधिकतम
यह समझ सकता है कि
आत्मा या परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है—पुरुषों में, बाघों में, हाथियों में,
चींटियों में, वृक्षों में, तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में।
110.
प्रश्न: अपरोक्ष अनुभूति क्या है?
उत्तर: यह ब्रह्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है।
यह आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान
है, जो निरंतर और गहन
ध्यान के द्वारा प्राप्त होता
है। 'अपरोक्ष' का अर्थ है—स्वतंत्र रूप से,
बिना किसी अन्य माध्यम के।
इसमें किसी बाहरी वस्तु से
सहायता लेने की आवश्यकता नहीं
होती, बल्कि स्वयं की आत्मा
से ही सहायता प्राप्त होती
है। अपरोक्ष अनुभूति के माध्यम से मनुष्य
प्रत्यक्ष रूप से जानता है—'मैं सर्वत्र हूँ।
मैं सभी वस्तुओं में हूँ। मैं मनुष्य
हूँ। मैं बाघ हूँ। मैं
चींटी हूँ। मैं हाथी हूँ।
मैं वृक्ष हूँ। मैं संपूर्ण
ब्रह्मांड हूँ।' वह सभी चीजों
को आत्मा में और आत्मा
को सभी प्राणियों में देखता है।
111.
प्रश्न: शरीर को आत्मा क्यों
नहीं माना जा सकता?
उत्तर: शरीर सीमित है। यह
जड़ है। यह अनेक भागों
वाला है। यह नश्वर है।
यह पंचमहाभूतों का प्रभाव है।
इसे भौतिक नेत्रों से देखा जा सकता
है। यह निरंतर परिवर्तनशील है।
इसलिए शरीर आत्मा नहीं हो
सकता। आत्मा शरीर से सर्वथा
भिन्न है।
112.
प्रश्न: प्राण को आत्मा क्यों
नहीं माना जा सकता?
उत्तर: प्राण जड़ है। जब
आप सो जाते हैं, तो यह किसी व्यक्ति
को आमंत्रित नहीं कर सकता।
यह विनाशी है और ब्रह्म
में लय हो जाता है।
इसे दिव्य दृष्टि से देखा
जा सकता है। यह परिवर्तनशील है। इसलिए
प्राण आत्मा नहीं हो सकता।
113.
प्रश्न: मन को आत्मा क्यों
नहीं माना जा सकता?
उत्तर: मन सीमित है। मन
जड़ है। मन विनाशी है।
यह सात्त्विक गुण का प्रभाव
है। इसे दिव्य दृष्टि से
देखा जा सकता है। यह
हमेशा परिवर्तनशील है। इसलिए मन
आत्मा नहीं हो सकता।
114.
प्रश्न: आत्मा का स्वभाव क्या
है?
उत्तर:
● आत्मा भूत, वर्तमान और भविष्य (सत) में विद्यमान रहता है।
● यह अनादि और अनंत (शुरू और अंत रहित) है।
● यह अचल, एकरस और एकरूप है।
● यह स्वयंभू (स्वतः विद्यमान) है।
● यह अखंड (बिना किसी भाग के) है।
● इसे भौतिक नेत्रों से नहीं देखा जा सकता (अदृश्य)।
● यह प्रथम कारण (परम कारण) और कारण रहित कारण (महाकरण) है।
● आत्मा चेतना (चित) है।
● यह स्वयं प्रकाशित (स्वयं-प्रकाश) है।
● यह पूर्ण (परिपूर्ण) और स्वयं ज्ञानस्वरूप (ज्ञानस्वरूप) है।
● यह सभी चीजों को प्रकाशित करता है (सर्व-प्रकाशक)।
● यह ज्ञानमय (बोधस्वरूप) है।
● आत्मा आनंद (आनंद) है।
● यह आनंदघन (आनंद का पुंज) है।
● इसका स्वरूप आनंदस्वरूप है।
● यह नित्य, निरुपाधिक और सर्वोच्च आनंदमय (नित्य, निरुपाधिक, निरतिशय आनंद) है।
परिशिष्ट II
'दशमस्त्वमसि'—'तू ही दसवाँ व्यक्ति है'
आजकल वैज्ञानिक हलकों में हर चीज़ को गणितीय रूप में व्यक्त करने का चलन है। यदि हम किसी प्राकृतिक नियम या घटना को गणितीय समीकरण के रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने उसे वैज्ञानिक ज्ञान के दायरे में ला दिया है और उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान कर दिया है। एक हद तक यह उचित भी है, क्योंकि सृष्टि की अभिव्यक्ति का आधार गणितीय ही है। हमारे पूर्वजों को भी गणित और सृष्टि की घटनाओं के बीच के इस संबंध का ज्ञान था, जिसे उन्होंने विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया। असंख्य विविध रूपों के मूल में केवल एक ही वास्तविकता है। केवल परम तत्व ही निरपेक्ष है और कोई अन्य नहीं। उसके नीचे जो कुछ भी प्रकट होता है, वह सख़्त रूप से सापेक्ष है। जब हम बुद्धि के माध्यम से सृष्टि में प्रकट होने वाली वास्तविकता की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें गणित से सहायता मिल सकती है, क्योंकि यह शुद्ध संबंधों का विज्ञान है, जिसमें कोई भौतिक तत्व नहीं होता, और यह विभिन्न प्रकट वास्तविकताओं के आपसी संबंधों पर कुछ प्रकाश डाल सकता है। यदि कहीं कोई असमानता या अंतर दिखाई देता है, तो उसका गहन अध्ययन हमें इन रहस्यों को और अधिक स्पष्ट करने में सहायता कर सकता है। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में, किसी प्राकृतिक नियम के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली असमानताओं और अपवादों से अधिक उपयोगी कुछ भी नहीं होता। इन्हीं अपवादों और विसंगतियों के विश्लेषण के द्वारा जिज्ञासु व्यक्ति के लिए नए ज्ञान के द्वार खुलते हैं।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 और ∞ (अनंत) वे गणितीय प्रतीक हैं, जो अस्तित्व में मूलभूत वास्तविकताओं के प्रतिनिधि हैं। 1 प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि सभी संख्याएँ 1 की क्रमिक वृद्धि से बनती हैं। हम देखते हैं कि 1 ही मूलभूत संख्या है, जो सभी अन्य संख्याओं का स्रोत है। शेष सभी संख्याएँ 1 के विस्तार से उत्पन्न होती हैं और विभिन्न रूपों में दोहराई जाती हैं। सभी संख्याओं के 1 से विकास की प्रक्रिया एक रोचक गणितीय समस्या है। केवल नौ मौलिक संख्याएँ होती हैं (1 से 9 तक) और इनके अतिरिक्त दो रहस्यमय गणितीय तत्व होते हैं—0 (शून्य) और ∞ (अनंत), जो वास्तव में कोई संख्याएँ नहीं हैं। ये ग्यारह गणितीय तत्व, जो अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, न केवल गणित की मूलभूत वास्तविकताएँ हैं, बल्कि किसी न किसी प्रकार से अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकताओं और उनके आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।
शास्त्र कहते हैं कि वास्तविकता केवल एक है और अद्वितीय (छां. उ. VI-ii-1)। इसलिए संख्या 1 की तुलना परम वास्तविकता, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, से की जा सकती है। यह एक ही वास्तविकता (1) अनेक रूपों में प्रकट होती है, जैसे गणित में अनगिनत संख्याएँ 1 से उत्पन्न होती हैं। श्रुति भी इस विचार की पुष्टि करती है: "यह सब वास्तव में ब्रह्म ही है" (छां. उ. III-xiv-1)। लेकिन अज्ञान के कारण हमें बहुलता दिखाई देती है।
यह अज्ञान क्या है? यह अज्ञान अविद्या कहलाता है, जो माया का उत्पाद है, बल्कि स्वयं माया ही है। माया वह है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है (या मा—स Maya)। यह ब्रह्म की एक अवर्णनीय शक्ति (अनिर्वचनीय शक्ति) है। यह न तो ब्रह्म की तरह वास्तविक है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर यह नष्ट हो जाती है, और न ही पूरी तरह से अवास्तविक है, जैसे खरगोश के सींग या बाँझ स्त्री का पुत्र, क्योंकि यह जगत के रूप में प्रकट होती है।
इस अनोखी प्रकृति के कारण, यह अज्ञानी लोगों द्वारा पूजनीय हो जाती है। गणित में शून्य को भी 'पूज्य' कहा जाता है। गणित में शून्य की स्थिति क्या है? यह एक अपरिभाषित, अज्ञात शक्ति है। यह केवल 'शून्य' नहीं है। इसके भीतर गणित के सभी नियम और संबंध अत्यंत समन्वित, किंतु अदृश्य रूप में विद्यमान रहते हैं। जब यह स्वतंत्र होता है, तो यह 'शून्य-मूल्य' का प्रतीत होता है, लेकिन जब यह 1 से किसी भी प्रकार जुड़ता है, तो यह हमें चकित कर देता है। निम्नलिखित उदाहरण इसे स्पष्ट करेंगे:
00000000.. ये शून्य बिना किसी मूल्य के हैं। 10000000.. ये शून्य अपनी स्थिति के अनुसार विभिन्न मूल्यों को धारण करते हैं। 00010000.. बाएँ ओर के शून्य बेकार हैं, लेकिन दाएँ ओर के शून्य मूल्य बढ़ाते हैं। 0.0000001.. दशमलव बिंदु के बाईं ओर का शून्य मूल्यहीन है, जबकि दाईं ओर के शून्य बहुत ही कम मूल्य रखते हैं। 0.1000000.. यहाँ दशमलव के दोनों ओर के शून्य बेकार हैं।
इस प्रकार, शून्य केवल 'कोई संख्या नहीं' या 'शून्य' की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि यह कुछ अद्भुत और अवर्णनीय करता है। इसलिए, शून्य की तुलना माया से की जा सकती है। अब, इन व्याख्याओं के आधार पर, संख्या 10 को विविध नाम-रूपों से युक्त इस ब्रह्मांड से तुलना की जा सकती है। यह केवल परम वास्तविकता (1) का ही एक 'आभास' है, जो माया (0) के कारण उत्पन्न होता है।
भारत में, प्राथमिक विद्यालय का छात्र भी 'लापता दसवें व्यक्ति' की कहानी जानता है, हालाँकि यह केवल एक कहानी के रूप में जानी जाती है, इसके गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ से अनभिज्ञ रहकर। कहानी इस प्रकार है:
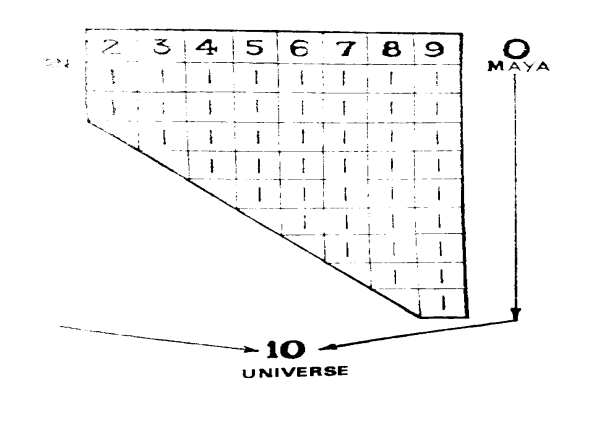
चित्र 15. ब्रह्म, माया और ब्रह्मांड
दस व्यक्तियों ने एक नदी पार की। दूसरी ओर पहुँचकर, उनमें से प्रत्येक ने गिनती कर यह सुनिश्चित करना चाहा कि सभी सुरक्षित पहुँच गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, उन्हें 'एक' व्यक्ति कम मिला। बार-बार गिनने के बावजूद, वे केवल 9 तक ही गिन पाते थे। अंततः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि दसवाँ व्यक्ति नदी में डूब गया है। वे रोने-चिल्लाने और अपने सीने पीटने लगे। तभी वहाँ एक सन्यासी आए और उन्होंने उनके दुःख का कारण पूछा। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। सन्यासी को स्थिति समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत कहा कि दसवाँ व्यक्ति मरा नहीं है, बल्कि जीवित है। यह सुनकर वे सभी राहत की साँस लेने लगे, फिर भी उन्हें 'गुमशुदा' व्यक्ति को लेकर संदेह था। सन्यासी ने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा किया और प्रत्येक को छूकर गिनना शुरू किया। जब वे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, तो उन्होंने कहा: "तू ही दसवाँ व्यक्ति है" (दशमस्त्वमसि)। यह सुनकर वे सभी प्रसन्न हो गए और अपने गंतव्य की ओर बढ़े।
इस हास्यास्पद स्थिति का दुखद पक्ष यह था कि गिनती करने वाला व्यक्ति स्वयं को भूल गया था।
यह कहानी चाहे जितनी भी अजीब लगे, लेकिन संसार के अधिकांश लोगों की स्थिति 'लापता दसवें व्यक्ति' से अलग नहीं है। बाह्य वस्तुओं की खोज में व्यक्ति स्वयं को ही भूल जाता है। यही 'अज्ञान' या 'अविद्या' की स्थिति है, जिसके कारण वह संसार के चक्र में बँधा रहता है। इस अज्ञान से केवल आत्मज्ञान के द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है, जो एक सच्चे गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है।
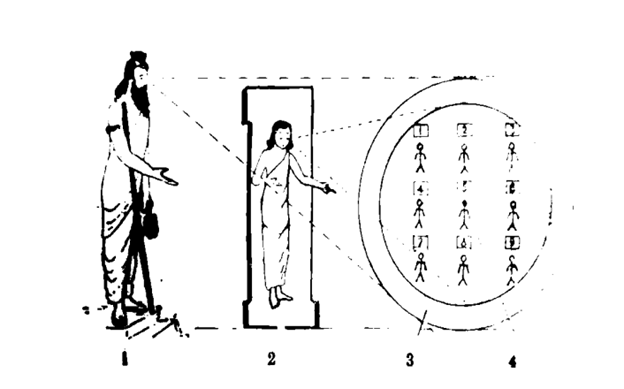
चित्र 16. तुम दसवें व्यक्ति हो
1. गुरु 2. लुप्त दसवाँ व्यक्ति (स्वयं या 1) 3. माया (0) 4. अनुभूति का ब्रह्मांड (माया द्वारा निर्मित स्वरूप)।
सारणी
वेदांत की श्रेणियाँ
या
चेतना का विकास दर्शाने वाला चार्ट
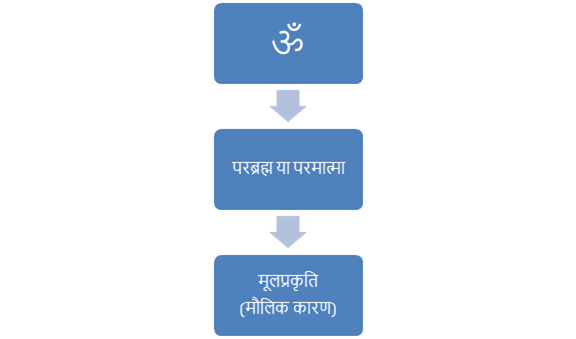
सत्व रज तम
सत्व शक्ति आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति
शक्ति आवरण प्रक्षिप्त शक्ति
चेतना चेतना की शक्ति अभानावरण
जीव या व्यक्तिगत आत्माएँ
84 लाख प्रजातियाँ
|
पंच तन्मात्रा |
|
(1) शब्द (ध्वनि या सूक्ष्म ध्वनि) |
(2) स्पर्श (स्पर्श) या सूक्ष्म वायु |
(3) रूपा या (सूक्ष्म अग्नि)
|
(4) रस (स्वाद) या (पानी)
|
(5) गंध (गंध) या (सूक्ष्म पृथ्वी)
|
|
सत्व का तन्मात्रा |
समष्टी 1
|
हृदय |
मन |
बुद्धि |
चित्त |
अहंकार |
|
व्यष्टिi 2 |
श्रोत्र (श्रवण शक्ति) |
त्वक (स्पर्श शक्ति) |
चक्षु (दृष्टि शक्ति) |
जिह्वा (स्वाद शक्ति)
|
घ्राण (गंध शक्ति)
|
|
|
रजस का तन्मात्रा
|
समष्टीti 3 |
व्यान (व्यापक) |
प्राण (श्वास लेना) |
अपान (श्वास छोड़ना)
|
समाना समानीकरण |
उदान (आरोहण) |
|
व्यष्टिi 4 |
वाक् (बोलने का अंग) |
पाणि (पकड़ने का अंग हथेली)
|
पाद (गति का अंग पैर)
|
उपस्थ (उत्पत्ति का अंग)
|
पायु (उत्सर्जन का अंग) |
|
|
तमस का तन्मात्रा
|
पंचीकृता 5 |
शब्द |
स्पर्श |
रूप |
रस |
गंध |
|
स्पर्श रूप रस गंध |
शब्द रूप रस गंध |
शब्द स्पर्श रस गंध |
शब्द स्पर्श रूप गंध |
शब्द स्पर्श रूप रस |
||
|
सृष्टि
|
I 6 |
आकाश मण्डल (स्थूल आकाश) 1 |
वायुमण्डल (स्थूल वायु) 2 |
आग (स्थूल अग्निi) 3 |
जल मण्डल (स्थूल जल) 4 |
स्थल मण्डल (स्थूल पृथ्वीi) 5 |
|
स्थूल प्रपंच
|
II 7 |
मानस पुत्र या मन से जन्मे (चार कुमार, दस प्रजापति आदि। |
जरायुज या जीवितप्रज्वलित या गर्भ से जन्मे (मानव प्राणी आदि)
|
अंडज या अण्डजंतु या अण्डजंतु (पक्षी आदि)
|
स्वेदज या पसीने से पैदा होने वाला (जूँ आदि) |
उदभिज या बीज जनित (पौधे आदि)
|
|
|
||||||
III ब्रह्मांड जिसमें 14 लोक (या विमान) शामिल हैं अर्थात (1) भू, (2) भुवः, (3) सुवः, (4) महः, (5) जनः, (6) तपः, (7) सत्य, (8) अतल, (9) वितल, (10) सुतल (11) तलातल। (12) महातल (13) रसातल और (14) पाताल। (पहले के सात उच्च क्षेत्र हैं और बाद के सात निम्न क्षेत्र हैं।) भोजन और अन्य भोग की वस्तुएं।
IV 1. अंतःकरण। 2. ज्ञान इंद्रियां। 3. प्राण। 4. कर्म इंद्रियां। 5. प्रत्येक तन्मात्रा का आधा भाग अन्य चार में से प्रत्येक के आठवें भाग के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण की इस प्रक्रिया को पंचीकरण या पंचमीकरण कहा जाता है। 6. पंच महाभूत या पाँच स्थूल तत्व। 7. पाँच प्रकार के शरीर।
विविध विवरण
नाम
|
शरीर |
कोश |
अंग |
स्थान |
इष्टदेव |
अवस्था |
व्यक्तिगत या व्यष्टि अभिमानी
|
सामूहिक या समष्टि अभिमानी
|
|
कारण शरीर |
आनंदमय कोश |
- |
- |
ब्रह्मा |
गहरी नींद या सुषुप्ति |
प्रज्ञा |
ईश्वर |
|
सूक्ष्म शरीर |
बौद्धिक या विज्ञानमय कोश |
बुद्धि और अहंकार |
आज्ञा चक्र (आँख का मध्य भाग भौंहें) |
रूद्र |
स्वप्नावस्था |
तैजस |
हिरण्यगर्भ |
|
मनोमय कोश |
मन |
पूरा शरीर |
दिक् |
स्वप्नावस्था |
तैजस |
हिरण्यगर्भ |
|
|
प्राणमय कोश |
पंच प्राण (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान) |
संपूर्ण शरीर विशेषकर अनाहत चक्र (हृदय चक्र) |
वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार |
जाग्रत अवस्था |
व्यष्टि प्राण |
समष्टि प्राण |
|
|
स्थूल शरीर |
अन्नमय कोश |
पंचमहाभूत (श्रोत्र (कान), त्वचा, चक्षु (नेत्र), जिह्वा (जीभ), घ्राण (नासिका)) |
कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका |
विष्णु |
जाग्रत अवस्था |
विष्व |
विराट पुरुष |
|
वाक् (वाणी), पाणि (हाथ), पाद (पैर), उपस्थ (गुप्तांग), पायु (गुदा) |
कंठ, जीभ, हाथ, पैर, गुप्तांग, गुदा |
चंद्र, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति |
|
|
|
धन्यवाद