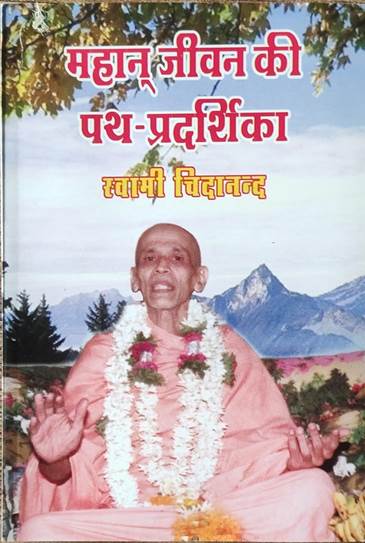
महान् जीवन की पथ-प्रदर्शिका
A GUIDE TO NOBLE LIVING
का हिन्दी अनुवाद
लेखक
श्री स्वामी चिदानन्द
अनुवादक
श्री शिवगोविन्द गुप्त, एम. ए.. साहित्यरत्न
प्रकाशक
द डिवाइन लाइफ सोसायटी
पत्रालय : शिवानन्दनगर-२४९१९२
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (हिमालय), भारत
www.sivanandaonline.org, www.dlshq.org
प्रथम हिन्दी संस्करण : १९७६
द्वितीय हिन्दी संस्करण : १९९१
तृतीय हिन्दी संस्करण : २०१७
(५०० प्रतियाँ)
© द डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसायटी
HC 21
PRICE 55/-
'द डिवाइन लाइफ सोसायटी, शिवानन्दनगर' के लिए
स्वामी पद्मनाभानन्द द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 'योग-वेदान्त
फारेस्ट एकाडेमी प्रेस, पो. शिवानन्दनगर-२४९१९२,
जिला : टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड' में मुद्रित।
For online orders and Catalogue visit : disbooks.org
प्रकाशकीय आमुख
आध्यात्मिक पुस्तक भले ही बुद्धि को सन्तोष प्रदान करे या न करे, पर यह तो निश्चित ही है कि वह आत्मा तथा प्रज्ञा की आवश्यकताओं तथा माँगों की पूर्ति अवश्य करती है। इस भाँति एक सन्त की, एक आत्मा के सन्देशवाहक की वाणी, जिस कालावधि में हम अपनी अन्तरात्मा के साथ होते हैं तो उस शान्त तथा भव्य क्षणों में हमसे बातें करती है। परम पावन श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज विचारशील मानव के अन्तर्तम प्रकोष्ठ में मौन रूप से बोलते हैं। उनकी वार्ता बड़ी आत्मीयता से साधक के हृदय को सीधे स्पर्श करती है।
श्री स्वामी केशवानन्द जी के श्रम तथा प्रेम के फलस्वरूप 'Path to Blessedness' (मुक्ति-पथ) के नाम से प्रथम संकलन तैयार होने पर विश्व-भर के भक्तों तथा साधकों की सेवा में उन्मोचन किया गया था जिसने उन्हें स्वामी जी की पुस्तक के संकलन के लिए यथेष्ट प्रोत्साहन तथा प्रेरणा प्रदान की। पूज्य गुरुदेव की परम भक्त फ्रांस की यवन्ने लेम्वाइन माता जी ने 'Path to Blessedness' (मुक्ति-पथ) पुस्तक के अनुक्रम में स्वामी जी की एक अन्य पुस्तक के उन्मोचन की व्यवस्था करने की अपनी उत्सुकता प्रकट की। भगवदिच्छा से ही श्री स्वामी केशवानन्द जी इस भव्य कार्य के सम्पादन के आंशिक रूप से माध्यम बने।
जीव के मोक्षदायक योग-मार्गों में भक्तियोग को जो गौरव प्राप्त है, प्रायः वैसा ही स्थान प्रस्तुत प्रकाशन को आध्यात्मिक साहित्य के क्षेत्र में उपलब्ध है। भक्तियोग राजपथगामिनी रेलगाड़ी के सदृश है जो विभिन्न स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों को उन्नयन करती है। वह उनकी सामाजिक प्रास्थिति तथा पद एवं योग्यता के भेद को न देख कर केवल उनके सवार होने तथा मार्ग तय करने की तीव्र उत्कण्ठा का ही विचार करती है। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति इस द्वार में प्रवेश कर सकता है। इस अनुपम योग-मन्दिर में सभी को प्रवेश करने का अधिकार है। प्राणी के परम मित्र तथा प्रेमी के प्रासाद के सम्मुख सारे सांसारिक भेद तिरोहित हो जाते हैं। भगवान् के सामने सभी को समान अधिकार प्राप्त है; क्योंकि दिव्यात्मा को सामाजिक भेद तथा मानव-निर्मित प्रतिबन्ध मान्य नहीं हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन की यह लघु पुस्तक नवछात्रों को अपनी इन पृच्छाओं का उत्तर देने के लिए अभिनन्दन करती है कि जीवन का यथार्थ उद्देश्य क्या है, योग का सही अर्थ क्या है, त्याग की सच्ची भावना क्या है तथा सदाचरण से प्रारम्भ कर पवित्रता से गुजरते हुए ईश्वरत्व में चरम परिणति क्योंकर हो सकती है? उन्नत साधक घोर संघर्षों तथा विरोधों के मध्य अपने सन्देहों तथा उभयापत्ति के अन्धकार के निवारणार्थ इस पुस्तक में इतस्ततः संकेन्द्रित प्रकाश-पुंज पाता है जिससे वह अकस्मात् निमेष मात्र में अपनी विरोधी समस्याओं का समाधान पाने में सफल हो जाता है। पूर्णत्व में अधिक उन्नत आत्मा इस साहित्य से हृदय से प्रसन्न हो उठेगी; क्योंकि यह दिव्य जीवन यापन सम्बन्धी विषय का प्रतिपादन करता है, भगवान् की महिमा, मोक्ष, आनन्द तथा शान्ति की चर्चा से समृद्ध है तथा श्री हनुमान् जैसे रामायण के प्रख्यात महान् भक्तों के अनुकरणीय आदर्शों तथा आधुनिक काल के मापदण्ड के अनुसार जीवन यापन करने वाले सन्तों की जाज्वल्यमान् प्रेरणादायी जीवनियों और आदर्शों का वर्णन करता है।
यह पुस्तक व्यापक रूप से प्रेरणादायी तथा पथ-प्रदर्शिका है। चूँकि इसका प्रतिपाद्य विषय अधिकांशतः सामान्य तथा स्वरूप किंचित् संक्षिप्त है; अतः योग की विविध प्रणालियों की प्रविधियों तथा अभ्यासों के विवरण में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से इस पुस्तक के प्रति उपगमन अनुपयुक्त ही होगा। इस पुस्तक को तो निवृत्ति तथा योग के पथ पर एक सन्त के सन्देश के रूप में ही श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। वैसे इस पुस्तक की उपयोगिता योग तथा वेदान्त की सामान्य पाठ्यपुस्तकों से कुछ कम नहीं है। उत्तरोक्त योग के किसी विशेष पहलू तथा प्रविधि का ही विशेषकर प्रतिपादन करती है तथा अपने कुछ चुने हुए प्रशिक्षार्थियों तथा अधिक कठिन प्रणाली के अनुयायी विद्यार्थियों की आवश्यकता तथा उनके लक्ष्य और उद्देश्य का ध्यान रखती है। इसके विपरीत इस प्रकार की पुस्तक की प्रथम तथा प्रमुख आवश्यकता सामान्य पाठकों तथा साधकों को है; क्योंकि यह अपने में जीवन को उसकी सभी परिधियों में सन्निहित करती है। सामान्य सिद्धान्त सदा ही प्रथम तथा विशेष बाद में आता है।
यह पुस्तक स्वामी जी के निबन्धों, लेखों तथा विविध अवसरों पर दिये गये संक्षिप्त भाषणों के रूप में उनके लेखों तथा प्रवचनों का संकलन है। प्रथम पाँच लेख प्रमुखालय आश्रम में दिये गये स्वामी जी के प्रेरणादायी प्रवचनों के उपयोजन हैं और ये जो अभी भी जीवन के यथार्थ अर्थ और उद्देश्य के अज्ञान के कारण आत्ममय जीवन के प्रति निद्रा में हैं, उनके लिए शंख-प्रघोष का कार्य करते हैं और उन्हें जाग्रत करने के पश्चात् भगवान् की ओर उनकी गति को पुनर्नुस्थापन के द्वारा उनके जीवन में नवीन शक्ति, साहस, आशा तथा ओज भरते हैं। तत्पश्चात् योग के मौलिक सिद्धान्तों तथा योग के विद्यार्थियों की प्राथमिक पूर्वापेक्षाओं की चर्चा करते हैं। बालसुलभ कुतूहल से जो योगमय जीवन को पुष्पाच्छादित (सुगम) पथ समझता है, उसे सावधान किया गया है तथा इस पथ को आकीर्ण करने वाली सम्भावित बाधाओं की ओर संकेत किया गया है। सामान्य मानवता के चतुर्दिक् के समाज के परिप्रेक्ष्य में योग के विद्यार्थी के आचरण के आदर्श को सेवा, समानता तथा सहानुभूति के रूप में दर्शाया गया है। हमें उन ज्ञानी ऋषियों के पदचिह्नों का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने आध्यात्मिकता के इस दुष्कर, दुरारोह पर्वतीय पथ को इससे पूर्व तय कर रखा है। जो शक्ति और सामर्थ्य का शाश्वत तथा अक्षुण्ण स्रोत है, जो पुरुषोत्तम है, जो सबका प्रेमी और मित्र है, जो सब पदार्थों में युगपत् विद्यमान सत्ता है, जो अपने प्रबल विश्वयोग द्वारा असंख्य रूपों में विश्वव्यापी शक्ति है, उससे अनन्त शक्ति प्राप्त कर सर्वशक्तिमान् प्रभु का भक्त अभेद्य हो जाता है। इस विषय को हनुमान् तथा रावण के भेद को चित्रित कर विशद तथा रोचक ढंग से दर्शाया गया है। देवी-उपासना की सच्ची धारणा तथा निम्न, अधम पाशविक प्रकृति की सभी वस्तुओं को विजित करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। इस पुस्तक में जहाँ भोगवादियों के आक्षेप का खण्डन किया गया है तथा त्याग की सच्ची भावना से चुनौती दी गयी है, वहीं पर कठोर जीवन यापन करने वाले एकान्तवासियों को उनके उत्तरदायित्व तथा पवित्र परम कर्तव्य का स्मरण कराने में भी ढील नहीं दी गयी है। मानव-मन, उसकी संरचना तथा मनोवैज्ञानिक कार्यशीलता का विस्तृत विश्लेषण कर व्यावहारिक साधना पर पर्याप्त संकेत दिये गये हैं। समय तथा सुविधा के अभाव की आड़ में अपने जीवन में भगवान् की पूजा-आराधना को स्थान न देने के प्रयत्न में असन्तोषजनक बहाने बनाने के लिए आधुनिक मनुष्य को छोड़ा नहीं गया है। हस्तगत कार्य में शरीर को संलग्न रखते हुए भी योग में मानसिक एकता प्राप्त करने की उसे विलक्षण साधना-विधि दी गयी है। इस लेख से ही पुस्तक का उपसंहार किया गया है। इस भाँति प्रत्यक्षतः असम्बद्ध शीर्षकों में परस्पर सम्बद्ध कराने वाली श्रृंखला की कड़ी उसी भाँति वर्तमान है जैसे मोती के मनकों को एक सूत्र में ग्रथित कर उन्हें सुन्दर हार का रूप दिया जाता है।
यदि यह सुप्रयोजनीय पुस्तक धर्माचरण, सत्य तथा भागवतीय चेतना में जीवन यापन हेतु गहन प्रेरणा प्राप्त करने की भावना से अध्ययन की जाती है तो संकलनकार का श्रम पूर्ण सार्थक समझा जायेगा।
-द डिवाइन लाइफ सोसायटी
अनुवादकीय
सद्गुरु श्री स्वामी चिदानन्द जी महाराज की पुस्तक 'A Guide to Noble Living' का अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी में अविकल अनुवाद 'महान् जीवन की पथ-प्रदर्शिका' के रूप में मेरे माध्यम से पूर्ण होने का सुअवसर प्राप्त हुआ, यह मैं अपना पुण्य एवं सौभाग्य मानता हूँ।
वैचारिक दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक तीन श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है :
(१) प्रथम में, संसार में आसक्त लोगों की अज्ञान-तमिस्रा से जाग्रत कर साधना हेतु आह्वान है। फिर साधना-पथ के अवरोध, भय समझा कर 'तृतीय कपालवत्' एवं 'सरल निष्कपट तथा सहनशील बनो' का सुझाव दे कर प्रोत्साहित किया गया है कि भक्त (ऐसा साधक) अभेद्य हो जाता है।
(२) द्वितीय में, अति-प्रवरता से 'हनुमान् एवं रावण में विरोधाभास' के सादृश्य द्वारा सन्देश प्रदत्त किया है कि अहंकार एवं अधर्म से युक्त रावण जैसे महाबली की शक्ति विकृत एवं असामाजिक हो जाती है जब कि विनम्र, सेवा एवं शरणागत भावमयी हनुमान् की शक्ति शिखरवत् प्रख्यात एवं सर्वग्राही बन जाती है। फिर साधु के कर्तव्यों (आदर्शों) का ज्ञान कराते हुए भोगवादियों के आरोपों का निराकरण और गुरु-शिष्य-सम्बन्ध पर हृदयस्पर्शी प्रकाश डाला गया है।
(३) तृतीय में, धर्म एवं संन्यास की महत्ता बताते हुए साधना-पथ में सफलता हेतु आवश्यक 'मानव-मन का विश्लेषण' सरल शब्दों में समझाया गया है। अन्तिम, किन्तु अति-महत्त्वपूर्ण, पूज्य स्वामी जी का पथ-प्रदर्शन, आज के व्यस्त मानव को 'आधुनिक मनुष्य के लिए साधना' के रूप में है जिसमें योग की जटिलताओं का निवारण कर शारीरिक साधना से मानसिक साधना पर विशिष्टता बतला कर साधना का पुनर्योजन किया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति के माध्यम से किया गया प्रत्येक कार्य ईश्वर-पूजा में रूपान्तरित होना सम्भव हो सकता है।
पूज्य स्वामी जी के भाषणों एवं लेखों का यह संकलन यदि हिन्दी भाषा-भाषी मनीषियों को किंचित् भी निवृत्ति एवं योग-पथ पर आरूढ़ होने में सहायक सिद्ध हो सका तो मैं अपना परिश्रम सफल समदूँगा। भावानुरूप यथावत् भाषान्तर प्रस्तुत करने की आदि से अन्त तक चेष्टा की गयी है। क्लिष्ट हिन्दी का यथाशक्ति निवारण किया गया है।
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!!
- शिवगोविन्द गुप्त
विषय-सूची
२. वासनाओं का उन्मूलन कर अपनी वासना-रहित आनन्दमयी आत्मा में विश्राम करो
५. आलस्य-वृद्धि हेतु बुद्धि का प्रयोग न करें
६. योग की आवश्यकता, आधार तथा उत्कृष्ट रचनात्मक तत्त्व
१०. मानवता की सेवा कर दिव्यत्व प्राप्त करें
१२. सरल, निष्कपट, विनम्र एवं सहनशील बनो
१३. उनके चरण-चिह्नों का अनुसरण करो
१५. हनुमान् और रावण में विरोधाभास
१७.ध्वंस निर्माण का अग्रगामी होता है
२४. आधुनिक मनुष्य के लिए साधना
१. अविच्छिन्न कड़ी
उच्च संस्कृति से सम्पन्न हमारे इस पावन देश भारतवर्ष में ईश्वरीय कृपा से निरन्तर धर्माचार्यों, सन्तों, भक्तों और आप्त पुरुषों की अविच्छिन्न धारा बहती रही है-ऐसे महापुरुषों की जो इस देश के वासियों को उनके वास्तविक जीवन-लक्ष्य का स्मरण कराते हुए मानव-जाति को प्रत्येक संकटपूर्ण क्षण में पथ-भ्रान्त होने से बचाते और कण्टकाकीर्ण मार्ग पर चलने को उत्साहित व्यक्तियों का मार्ग-प्रदर्शन करते थे। यदि हमारे प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात किया जाये तो ऐसा कोई युग नहीं मिलेगा जो मानवता को सदैव सजग रहने की तथा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नित्य स्मरण रखने की उद्घोषणा के साथ सत्य की ध्वजा फहराने वाले अवतारी पुरुषों से रिक्त रहा हो।
उन्होंने कभी भी बौद्धिक क्रिया-कलाप और वैचारिक उछल-कूद मात्र से किसी परिणाम की घोषणा नहीं की, बल्कि प्रत्यक्ष अन्तर्ज्ञान के द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कार की आधिकारिक घोषणा की। अतः जो-कुछ भी इन प्राचीन ऋषियों-मुनियों ने उपनिषदों में घोषित किया है, वह उनके अन्तस्तल में परब्रह्म की प्रत्यक्षानुभूति से है। उन्होंने अपने विचारों के समर्थन हेतु कोई तर्क उपस्थित करने की ओर ध्यान नहीं दिया और न ही उनकी स्वीकृति के इच्छुक हुए। उन्होंने जो सत्य के रूप में जाना, उसे ही निर्भीकतापूर्वक वर्णन किया। और, वह क्या है जो उन्होंने घोषित किया ? वह यह है :
ओ! अजर अमर बच्चो महान् !
नहिं तुम शरीर यह नष्टप्राय,
नहिं मन जो परिवर्तन कराय,
नहिं बुद्धि जो तर्कों में रमाय,
बस, स्वामी इस सबके सुजान।। ओ! अजर अमर...
तुम परम चेतना के चेतन,
तुम अनासक्त द्रष्टा केवल,
तुम मन बुद्धि से दूर अगम,
तुम आत्म-चेतना परा-ज्ञान।। ओ! अजर अमर...
भिन्न पृथक् नहिं काय-रूप,
मन बुद्धि ना हो, प्राण-स्वरूप,
पहिचानो यह 'शिव' सत्य रूप,
कर आत्मबोध में सजग वास ।। ओ! अजर अमर…
उन्होंने इस महान् अनुभव की ओर ले जाने वाला पथ भी दिखलाया। हमें अपने प्राचीन ऋषियों के सच्चे उत्तराधिकारी और भारतवर्ष की योग्य सन्तति के रूप में, कभी भी जीवन के परम लक्ष्य को द्रष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए जो कि ईश्वर-साक्षात्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। तथाकथित भौतिक उत्कर्ष के नाम पर हममें से कोई भी विदेशी सभ्यता का शिकार न बन जाये।
वृक्ष की श्रेष्ठता अन्ततोगत्वा उसके मधुर या कड़वे फलों से ही ज्ञात की जाती है। विगत दो महा-विश्वयुद्ध, अति आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान की छाया में पल्लवित तथाकथित प्रगतिशील सभ्यता के नाम पर ध्वंसकारी आतंक के प्रमाण हैं।
मैं ऐसे भ्रामक ज्ञान को काफी दूर से नमस्कार करना चाहूँगा तथा स्वयं को सहस्र बार अज्ञानी कहलवा कर आत्मविकासोन्मुख संस्कृति और पूर्वजों से प्राप्त विरासत से दृढ़तापूर्वक संलग्न रहना पसन्द करूँगा जो मुझमें पवित्रता, मनुष्यता, देवत्व, चरित्र, निष्ठा, निःस्वार्थता और मनुष्य मात्र के लिए प्रेम भरती है।
बन्धुओ, सावधान! धर्म और आध्यात्मिकता से शून्य वैज्ञानिक ज्ञान विश्व के दुर्भाग्य को शीघ्र ले आयेगा; क्योंकि यह ज्ञान भ्रष्ट मनुष्य की सबको निगलने वाली पाशविक वृत्ति के हाथ में दिया गया है जिसमें स्वयं ही आत्मघातक शक्ति है।
अधिकार सचमुच भ्रष्ट करता है और पूर्ण अधिकार पूर्णतया भ्रष्ट करता है।
अतएव, अपने चरित्र-निर्माण, भद्रता, दिव्यता और स्वरूप की खोज के लिए गहन रुचि के प्रमुख कर्तव्य की अवहेलना न करें।
२. वासनाओं का उन्मूलन कर अपनी वासना-रहित आनन्दमयी आत्मा में विश्राम करो
आध्यात्मिक साधक नित्य ईश्वर के निकट और निटकतर आता जाता है। दिन-प्रति-दिन उसका आध्यात्मिक प्रयत्न उसके लिए माया एवं भौतिक बन्धनों से छुटकारा लाता है। प्रत्येक विगलित इच्छा छुटकारे की प्रगति को नवीन शक्ति देती है। यह आन्तरिक सुख के भण्डार में एक नवीन वृद्धि है।
वासनाओं के क्षयीकरण हेतु कुछ उपाय यहाँ इस प्रकार हैं :
(१) आत्म-नियन्त्रण-अनावश्यक आवश्यकताओं, क्रिया- कलापों और मिलने-जुलने को कम कर दो। मित्रों से अत्यधिक सम्पर्क और व्यर्थ मिलना पुरानी आदतों और पूर्व-संस्कारों की वृद्धि करते हैं। अतः जहाँ तक भी सम्भव हो, सांसारिक सम्बन्धों को घटा देना चाहिए। कुछ शुद्ध संकल्प लाओ और जहाँ के तहाँ (तुरन्त) ही अस्वीकार करो और कहो, 'नहीं, यह मुझे नहीं चाहिए; क्योंकि इससे मेरी आध्यात्मिकता को कोई सहायता नहीं मिलने वाली है।' शुद्ध बुद्धि वालों से परामर्श लो। इससे वांछित क्षणों में आपको निश्चित संरक्षण मिलेगा। आप शनैः-शनैः इन्द्रिय-विषय को विष-तुल्य और भ्रमात्मक माया की चालाक पकड़ के रूप में देखने की प्रवृत्ति का विकास करेंगे। फिर अपने आध्यात्मिक कल्याण हेतु आप स्वभावतः उनका तिरस्कार कर देंगे।
(२) असावधानी-पिछले संस्कार प्रच्छन्न शक्तियों के समान हैं और कुण्डल्याकार गुप्त ऊर्जा के समान हैं जो कभी-कभी प्रचण्ड रूप धारण कर लेते हैं और मन में भीषण उथल-पुथल पैदा कर और उसे पूर्णतया भ्रान्त और आकुल कर वासनाओं का रूप लेने को बाध्य कर देते हैं। इसी को विषयाकार वृत्ति कहते हैं। इसलिए सजगता (सावधानी) का आश्रय लेना चाहिए। मन को किंचिन्मात्र भी ढील नहीं देनी चाहिए।
(३) असहयोग-समस्त इन्द्रियों को शनैः-शनैः उनके स्व-स्व आनन्द-केन्द्र से वापस लौटा लेना चाहिए। यदि आप समस्त इच्छाओं को अस्वीकार करते जायेंगे तो वे स्वाभाविक मृत्यु (क्षय) को प्राप्त होंगी।
अतः आत्म-नियन्त्रण की इस नैरन्तरिक प्रक्रिया को चलाते जाओ और समस्त वासनाओं के विजेता बन जाओ। इस प्रकार मन से समस्त वासनाओं को धो कर मन को स्वच्छ करने पर ही साधक विशुद्ध चेतना में, परमानन्द और आत्मानन्द में विलास करता है।
३. साधक और संसारी पुरुष
वासना-त्याग के बिना मनोनाश प्रभावी नहीं हो सकता और बिना मनोनाश के कैवल्य अथवा अमरत्व की आशा नहीं की जा सकती। पूर्णतया इच्छा-रहित स्थिति पूर्ण शान्ति और आनन्दमयी होती है।
आध्यात्मिक साधक शनैः-शनैः अपने मन को क्षीण, इच्छाओं को न्यून और अन्त में समस्त सांसारिक वासनाओं का सम्पूर्ण नाश कर संसार से आत्यन्तिक छुटकारा प्राप्त करता है।
दूसरी ओर संसारी मनुष्य अपनी वासनाओं की पोटली में प्रतिदिन नवीन वृद्धि करता है और इस प्रकार संसार में फँसने की प्रक्रिया को पुष्ट करता है; अन्त में वह अपने-आपको बन्धन की स्थूल श्रृंखला से जकड़ा हुआ पाता है। वह फन्दे में फँसता है, धोखा खाता है और माया से ग्रसित हो जीवन-लक्ष्य को चूक जाता है।
इस प्रकार आध्यात्मिक साधक और संसारी मनुष्य तुलना में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के समान पृथक् पृथक् स्थिति में होते हैं। एक उच्च प्रकृतिवश ऊँचाई की ओर खिंचाव से ऊर्ध्व विचरण करता है, दूसरा निम्न प्रकृतिवश नीचे की ओर खिंचाव से स्वयं को संसार-गर्त में फेंक देता है।
४. उठो और पुरुषार्थ करो
केवल आज का दिवस आपका है। कल व्यतीत हो चला। आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं। अतः वर्तमान क्षण, वर्तमान जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करो। उठो और पुरुषार्थ करो। आज का दिन परोपकारमय एवं पूजामय व्यतीत करो। व्यर्थ गपशप में, निन्दा-चुगली करने में, पिशुनता में, व्यर्थ की आशाओं और बातचीत में अपना अमूल्य समय नष्ट न करो। अन्यथा पश्चात्ताप और रुदन करते हुए संसार से प्रयाण कर जाओगे।
कौन जानता है कि यह स्वर्णिम अवसर पुनः आयेगा या नहीं? अतएव, जब प्रत्येक पदार्थ महान् आदर्शों के प्रकाशमान शिखरों तक उठने (उन्नतिशील होने) के लिए सहायक है तो सावधान होइए कि प्रमादवश उत्साह कहीं ठण्ढा न पड़ जाये। अतः कल के लिए मत टालो। टालने का अर्थ है अवसर को सदा के लिए खो देना। इसे स्मरण रखें।
संसार के प्रति हम सबका दृष्टिकोण शुभ का, मैत्री का एवं निःस्वार्थता का होना चाहिए। हमें दूसरों के कल्याण, शान्ति एवं प्रसन्नता के लिए जीवन यापन करना चाहिए; यहाँ तक कि उनके लिए भी जो हमें धोखा देते तथा आघात पहुँचाते हैं। प्यारे साधक! चिन्ता न करो; क्योंकि यह तुम्हारा चिरस्थायी निवास नहीं है। तुम एक अमर प्रकाशमान मूल-निवास हेतु तीव्रगामी यात्री हो। अतः पथ के मध्य, जब कि यहाँ तुम कुछ ही समय के लिए हो, दूसरों में थोड़ी प्रफुल्लता लाने, अपने पड़ोसियों की चिन्ता, भय, असुविधाओं को घटाने और उनके नयनाश्रु पोंछने का प्रयत्न करो। अपने सभी साथियों की उदासी, निराशा एवं दुःख जहाँ तक भी तुम दूर कर सको, करो।
यह तुम्हारे बहिर्जीवन का दृष्टिकोण होना चाहिए।
परोपकार के माध्यम से तुम उस एक परमात्मा की पूजा करते हो जो सर्वान्तर्वासी है। 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः'-वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियों की हृदयरूप गुहा में छिपे हुए हैं। अतः निर्धन के प्रति सहानुभूति रखो और उस (ईश्वर) को उस (ईश्वर) की छोटी-से-छोटी रचना में अवलोकन करने का प्रयत्न करो।
जहाँ तक हमारे आन्तर जीवन की बात है, यह हमारे दिव्य सम्बन्धों के प्रति सतत सजग एक यौगिक जीवन होना चाहिए।
दैनिक प्रार्थना, पूजा, भजन-कीर्तन और जप-यज्ञ द्वारा सत्त्वगुण की अभिवृद्धि करो। यह जप-यज्ञ निश्चित, सुरक्षित एवं सरलतम है। विशेषतः यह कलियुग के लिए समीचीन मार्ग है।
अन्तः तमस् (निष्क्रियता) एवं शैथिल्यवश कभी-कभी मन प्रयत्न करने से इनकार करेगा। इस तमस् (आलस्य) के आगे आत्म-समर्पण न करें। इसे रचनात्मक कार्यकलाप, अध्ययन एवं कीर्तन द्वारा दूर करें।
'उठो और पुरुषार्थ करो' और इसके द्वारा प्रमाद भगाओ।
५. आलस्य-वृद्धि हेतु बुद्धि का प्रयोग न करें
एक विनोदमयी किन्तु अर्थगर्भित विशिष्ट घटना मेरे मस्तिष्क में स्फुरित हुई है जो कुछ सीमा तक आधुनिक विज्ञान और तकनीक के समस्त तथाकथित प्रगति के आवरण में छिपे विषाक्त एवं अनोखे उद्देश्यों को स्पष्ट करती है।
एक सज्जन ने अपने उत्साही पुत्र से, जो उस समय किसी तकनीकी संस्था का छात्र था, पूछा- 'प्रिय पुत्र ! यदि तुम एक अच्छे और प्रसिद्ध इंजीनियर बन जाओगे तो क्या करोगे ?' लड़के ने उत्तर दिया, 'प्रिय पिता जी, मैं एक मशीन का आविष्कार करूँगा जो बटन दबा देने मात्र से मुझे मेरी मनचाही सभी वस्तुओं को देने की क्षमता रखती हो।' पिता ने वही प्रश्न अपने द्वितीय पुत्र से किया जो अपने अग्रज के आदर्शों का पूर्णतया अनुकरण कर रहा था-'जब तुम भी आधुनिक तकनीक में, जैसी कि तुम्हारी तीव्र महत्त्वाकांक्षा है, निष्णात हो जाओगे, तब तुम्हारी क्या करने की आकांक्षा होगी?' और उत्साही किशोर ने अविलम्ब उत्तर दिया- 'पिता जी, मुझे एक दूसरी मशीन का आविष्कार करना होगा जो मेरे बड़े भाई की अद्भुत मशीन का बटन दबाने हेतु प्रयुक्त होगी और इस प्रकार हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए प्रायः ही बटन दबाने के झंझट से हमें बचाती रहेगी।'
यह वैज्ञानिक मस्तिष्कों के आधुनिक विचारों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इतना अधिक तमस् या जड़ता मनुष्य के स्वभाव में, विलास एवं अभिशाप के रूप में प्रवेश कर गयी है कि एक समय आता है जब एक बटन दबाने में भी वह हिचकिचाने लगता है। बुद्धि को अधिक-से-अधिक शारीरिक आराम एवं मशीनों के आविष्कार में, यहाँ तक कि दैनिक कार्यों में भी बुद्धि लगाने के बजाय इस अमूल्य शक्ति का उपयोग सत् तथा असत् का विवेक करने में लगाया जाये। बुद्धि को शाश्वत, अमर, अजर एवं पूर्ण आनन्दमयी आत्मा की खोज में निर्देशित होने दो और जीवन को इस प्रकार रूपान्तरित कर दो कि वह भागवत सम्पर्क से प्रसूत सत्य और अक्षय सुख का आनन्द प्राप्त करे। अन्त में समस्त भयों और पीड़ाओं से रहित परमानन्द के धाम में विश्राम करो।
६. योग की आवश्यकता, आधार तथा उत्कृष्ट रचनात्मक तत्त्व
योग के उद्भव का आधार मानव की वह आवश्यकता है जिसे उसने समस्त शोक और पीड़ाओं से छुटकारा पाने, सीमित अस्तित्व द्वारा लाये गये बन्धनों से सदैव के लिए अपने को मुक्त करने तथा समस्त भयों, यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु पर भी अन्ततः विजय प्राप्त करने के लिए अनुभव की। इस महान् समस्या हेतु योग एक कृतात्मक निदान प्रस्तुत करता है। योग स्पष्टतः वर्णन करता है कि मनुष्य स्वरूपतः आनन्द, पूर्ण शान्त एवं मुक्त रूप है। स्वयं की सभी के पूर्ण स्रोत असीम के साथ एकत्व के बोध की कमी ही भौतिक प्रपंच में लिप्त होने का कारण है जिसे पार्थिव जीवन कहते हैं। वास्तविक ज्ञान की पुनर्प्राप्ति और दिव्यत्व के साथ एक बार पुनः चिरन्तन एकता का अनुभव करना ही वास्तव में योग-साधना है। भौतिक जीवन की कमियों एवं अपूर्णताओं पर विजय पाने के साधन और इस प्रकार परमात्मा से एकत्व की अनुभूति ही इसकी संरचना का गठन करते हैं। योग प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार निम्न प्रकृति की अपूर्णताओं को जीता जा सकता है और मन तथा इन्द्रियों पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किया जा सकता है। योग की समस्त तकनीकियों (कारीगरी) में पूर्ण आचार एवं नैतिक पवित्रता वांछनीय है। पवित्रता यौगिक जीवन की आधारशिला है। कोई भी व्यक्ति बुरा होने के साथ-साथ योगाभ्यास में प्रयत्नशील नहीं हो सकता। योगाभ्यास में प्रयत्नशील कोई भी व्यक्ति अपने को दूसरों के लिए अपवित्र, अश्रद्धालु, असत्यवादी, धोखेबाज और हानिकारक नहीं होने दे सकता। जब तक आन्तरिक पर्यावरण अपूर्ण है, कोई भी आध्यात्मिक अनुभव सम्भव नहीं हो सकता। जब तक नैतिक सद्गुण गहराई तक किसी में रोपा न गया हो, कोई भी धर्माभ्यास या सच्चा आन्तरिक जीवन सम्भव नहीं। अपने को अच्छाई, पवित्रता, सत्यता एवं निःस्वार्थता में आरोपित करना होगा। योग की आधी प्रक्रिया तो इस प्रकार आदर्श नैतिक आचरण में पूर्णतया प्रतिष्ठित करने में ही है। जब यह आधार स्थापित कर लिया हो तब योग की तकनीक का प्रयोग सूखी दियासलाई की तीली को दियासलाई में रगड़ने से तुरन्त ज्वाला की लपट निकलने के समान है। इस आधार के बिना भीगी दियासलाई की तीली को साबुन की बट्टी पर रगड़ने के समान होगा जिसका परिणाम कुछ भी न होगा।
यौगिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट साधन ईश-कृपा है। इसे आप जो चाहे कह लें। केवल समस्त अस्तित्व के स्रोत रूप परम तत्त्व की कृपा में मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव का और अमर देवत्व का अनुभव करता है। वे समस्त अभ्यास से पूर्ण होते हैं जो मनुष्य को परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं और उस सत्ता में एकत्व के साथ विलय कराते हैं। यही योग का उद्देश्य है।
७. साधना
इस पार्थिव जगत् में हमारे आने का एकमात्र अभिप्राय साधना है और यह भूलोक ही एक ऐसा स्थान है, जहाँ आत्म-साक्षात्कार की साधना की जा सकती है।
साधना का अर्थ है सम्यक् जीवन, ईश्वर प्रकीर्णित जीवन-चर्या। अपने हृदय से असत्यता को आमूल नष्ट कर सत्य के जीते-जागते साकार रूप बनो।
तुम सदा पवित्र और कलंक-रहित हो। अपने विचारों में, शब्दों में, इच्छाओं के आकार में और अपने दैनिक जीवन के आन्तरिक उद्देश्यों में सतत पवित्र और निष्कल्मष स्वभाव को व्यक्त करो। इसका अभ्यास करो, इसमें निवास करो, इसकी किरणें विकीर्ण करो, यही साधना है। तुम सत्य हो, परम सत् हो। इस सत्य को व्यक्त करो।
जो-कुछ तुम हो, तुम्हारा जीवन उसका विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। जो-कुछ तुम हो, वही दिखो। यही अनिवार्य साधना है। यह दिव्य जीवन यापन का, विचारों, शब्दों और कार्यों में दिव्यता की अभिव्यक्ति का सरल मार्ग है।
दिव्य जीवन यापन ही श्रेष्ठ साधना है, जहाँ प्रत्येक क्रिया, विचार और वाणी दिव्यत्व के गुण से अनुप्राणित रहते हैं।
परिस्थितियों पर विजयी बनो। कार्यरत रहने पर भी इस आन्तरिक जागरूकता को न त्यागो। प्रत्येक क्षण सभी वस्तुओं में इसे दृढ़तापूर्वक अंगीकार करो। अपने मन के विजेता, अपनी इच्छाओं के दमनकारक तथा अपने भाग्य के विधाता बनो; क्योंकि तुम स्वामी हो।
आप श्रेष्ठ सच्चरित्र का विकास करें और भद्रता व शुद्धता, सत्यता व पवित्रता एवं नैतिकता के पथ पर, विशेषतः उस यशस्वी लक्ष्य की ओर चलो जो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। यह तुम्हारा जन्म-सिद्ध अधिकार है जिसकी माँग तथा अनुभव तुम इसी जन्म में कर सकते हो। इसे भविष्य के लिए स्थगित न करो तथा कर्मनिष्ठ बनो।
८. अवरोध-त्रय
आप अपने हृदयोद्यान में दिव्य गुणों के पुष्पों को उगायें। सद्गुण से ही पवित्रता की ओर, पवित्रता से ईश्वरत्व की ओर तथा ईश्वरत्व से ईश्वर-साक्षात्कार की ओर अग्रसरित होना सम्भव होता है। व्यक्ति अपवित्रता से पवित्रता, पवित्रता से शुद्धता तथा शुद्धता से परम उदात्त आध्यात्मिक अनुभव की ओर प्रगति करता है।
जीवात्मा को परब्रह्म के अनुभव के प्रकाशवान् शिखर पर आरोहण करने में साधना के क्रियात्मक पथ में तीन अवरोध मिलते हैं, जिनको जीतना ही पड़ता है। प्रथम है स्थूलता की अवस्था जो शरीर-रूपी घर से पूर्ण तादात्म्य का परिणाम है। यह एकरूपता ही हमें 'हम यह शरीर हैं और यह शरीर हम हैं' ऐसा अनुभव कराती है।
'मैं यह शरीर नहीं हूँ', इस तथ्य को कितने ही शब्दों में मुखरित किया जाये तो भी अगले ही क्षण हमारा वास्तविक जीवन और व्यवहार वस्तुतः हमारे देहाध्यास को प्रदर्शित करता है। यदि कोई अकस्मात् आ कर यह कहे, 'हे मूर्ख, तू अपना समय वहाँ बैठ कर बरबाद कर रहा है। क्यों नहीं जा कर तू काम करता है?' तब तुम्हारा पारा ऊपर चढ़ जायेगा और तुम क्रोध की स्थिति में होगे। वेदान्त विलीन हो जायेगा और बुद्धि दीर्घकालीन स्वभाव के कारण क्रोध के आवेश के वशीभूत हो जायेगी। अब मन, शरीर तथा सभी द्वन्द्वों से परे रहने वाला अनन्त आत्मा एवं सच्चिदानन्द स्वरूप अमुक व्यक्ति तुरन्त उठ खड़ा होता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। आपका मन विद्रोह कर बैठता है। यह उद्वेलित हो सोचता है, 'मैं इस व्यक्ति से कैसे प्रतिशोध लूँ?' क्रोधामि बढ़ती है और मन उत्तेजित हो जाता है और तुम चाहते हो कि जाऊँ और उसकी नाक पर एक मुक्का जमा दूँ। तुमने पूर्णतया भुला दिया है, 'मैं नाम और रूप से परे एवं पूर्ण प्रकार से निःशेष तथा आनन्दघन, शान्त और नित्य सुखमय सच्चिदानन्द आत्मा हूँ।'
क्रोध, जो मल (मनःदोष) का एक प्रकार है, के कारण अपने सुन्दर आत्मिक स्वभाव की स्थिति से स्वभावगत कुरूपता और अधःपतन का यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार लोभ, वासना, स्वार्थ, उद्दण्डता, डाह, ईर्ष्या आदि भी मानव-स्वभाव के दोषों (मलों) का गठन करते हैं और जब तब उद्भूत हो मन को वश में कर लेते हैं। तब आत्मबोध मलिन या प्रच्छन्न हो जाता है और क्षुद्रता, बेईमानी, असहनशीलता, अहंकार तथा 'मुझे इस प्रकार सम्बोधित करने का इसने साहस कैसे किया' जैसे विचार मस्तिष्क में आ जाते हैं।
ये सभी मन के दोष कहलाते हैं जो मानव-व्यक्तित्व के आधारभूत दूषण हैं। ये दोष सदैव मानव-व्यक्तित्व को दूषित करते हैं। यदि ज्ञान के उच्च स्तर पर तुम्हें उठना है तो इनको दूर करना आवश्यक है।
ये मन के दोष सदैव मन को उत्तेजना और क्रियाशीलता की स्थिति में डाल देते हैं। वे कभी मन को शान्त और स्थिर नहीं रहने देते। मन के ये स्थूल दोष जब तक मन को बाह्य अनात्मिक कार्यों में प्रत्येक क्षण खींचते हैं, आप श्रेष्ठतम वास्तविकता के विचार की अखण्डित धारा में स्थिर रहने की आशा नहीं कर सकते।
मनः दोष के कारण मन अशान्ति, बहिर्मुखता और उद्वेग की स्थिति में विचलित रहता है। यह द्वितीय अवरोध है जिसे विक्षेप कहते हैं, इस पर भी विजय पानी होती है।
तुम्हारे मन के और भी गहरे अन्तराल में एक तृतीय अवरोध है जिसे आवरण कहते हैं। तुम्हारी चेतना की गहराइयों पर यह एक रहस्यमय परदा है जो तुम्हें तुमसे उच्च स्वभाव से अनभिज्ञता की स्थिति में ग्रसित किये रहता है। आवरण ही अनभिज्ञतावश आधारभूत अज्ञानता का कारण है। यह आवरण-शरीर और मन मैं हूँ-के तादात्म्य भाव से निर्मित है।
मल, विक्षेप तथा आवरण-इन तीनों को शनैः-शनैः सीढ़ी-दर-सीढ़ी विधिवत् पद्धति से जीतना है और तब आप अकस्मात् आत्मज्ञान का प्रकाश देखेंगे और आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करेंगे। आपको यह उत्कृष्ट आत्मीय अनुभव होगा।
प्रतिपक्षीय भावना द्वारा आधारभूत दोषों को दूर किया जा सकता है। जब आपको तम हटाना होता है तब आप क्या करते हैं? आप अँधेरा झाड़ने के लिए अथवा अन्धकार दूर करने के लिए झाडू या कूँचा तथा थैला नहीं लाते। आप अन्धकार-विलोपन हेतु सकारात्मक (प्रतिपक्षीय) गुण प्रकाश को लाते हैं।
जिस क्षण सकारात्मक प्रतिपक्षीय गुण का प्रवेश होता है, अभावात्मक गुण विलीन हो जाता है; क्योंकि अभावसूचक गुण का कोई आधार नहीं होता। अभावसूचक गुण अपने-आपमें कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता। इस पर अत्यधिक सावधानी से ध्यान दो। अभावात्मक गुण वास्तव में कोई सामर्थ्य नहीं रखते। वे केवल सद्गुणों की अनुपस्थिति को व्यक्त करते हैं। 'वह एक बड़ा असत्यवादी है' कहने का तात्पर्य है कि वह अपने में सत्यता नहीं रखता। असत्य नाम की कोई वस्तु नहीं; किन्तु उस व्यक्ति में सत्य का अभाव है। जिस क्षण वह दृढ़तापूर्वक यह कहते हुए सत्य का स्वागत करता है, 'मैं सत्यनिष्ठ होने का प्रयास करूँगा' तभी से उसको झूठा नहीं कहा जा सकता।
घृणा एक सकारात्मक गुण नहीं है। घृणा जैसी नाम की कोई वस्तु नहीं। इसका आशय है कि वहाँ प्यार नहीं है, दयालुता नहीं है। अतः यह केवल प्यारहीन दशा की ओर संकेत करती है और जो प्रेम तथा करुणा का सृजन करता है, उसमें घृणा बिलकुल नहीं होगी। जिस क्षण प्रेम आता है, घृणा तिरोहित हो जाती है; क्योंकि सकारात्मक वास्तविक है और नकारात्मक अवास्तविक। जब सकारात्मक गुण का सृजन किया तो नकारात्मक विलुप्त हो जाता है।
अतः स्मरण रखो कि गुणों का सृजन आत्म-संस्कार का प्रधान अंग है जो आध्यात्मिक विकास और दिव्य अनुभव की ओर ले जाता है। यह नींव रखने के समान है। यदि तुम्हें जंगली भूमि-खण्ड पर एक उद्यान लगाना है तो प्रथम कार्य जो तुम्हें करना है, जंगली घास-पात, गोखरू, कँटीले पौधे समूल निकाल डालना और ऐसी अनावश्यक नीचे उगी वस्तुएँ हटा देना। तब तुम्हें कंकड़ों और पत्थरों को हटा कर जमीन तैयार करनी होगी और तत्पश्चात् भूमि को उपजाऊ बनाना होगा।
इस प्रकार आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया तुम्हें सभी आसुरी एवं अनात्मिक वृत्तियों को दूर कर तथा लोलुपता, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार तथा उद्दण्डता जैसे निर्मम तथा पाशविक स्वभाव का अतिक्रमण कर समस्त अवांछनीय तत्त्वों से मुक्ति पाने के लिए कार्य करना होगा। तब तुम्हें अपने हृदयोद्यान में सद्गुणों के पुष्पों को उगाना होगा। केवल मात्र तभी तुम ईश्वरत्व की स्थिति में उठ सकोगे। शुद्धता ईश्वरत्व की अनुगामी है। दिव्य गुणों के सृजन में प्रत्येक व्यक्ति को अतीव उत्साही होना चाहिए। गुणों के सृजन तथा दुर्गुणों के विलोपीकरण से मन के भ्रमित, उद्वेलित और उद्विग्न होने के स्वभाव का क्षयीकरण हो जाता है। प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अज्ञानता का आवरण एक ओर हट जाता है। अब आप वास्तविक बोध की स्थिति में पहुँच जाते हैं। अब आपका अनुभव एक पूर्ण आध्यात्मिक आनन्द और शान्ति का होता है। अब आप आध्यात्मिक चेतना या दिव्य आनन्दातिरेक के उस महान् अनुभव का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं? आप केवल कहेंगे, 'मैं सच्चिदानन्द हूँ।’
९. पथ नहीं गुलाब-प्रसूनों सा
कोई भी उपयोगी वस्तु उतनी ही मात्रा में पीड़ा एवं कष्ट उठाये बिना प्राप्त नहीं हो सकती। कोई स्थायी आदर्श भी बिना श्रम तथा स्वेद के प्राप्त नहीं होता। पौधा बनने हेतु बीज फूटता और विनष्ट हो जाता है। पुष्प मधुर फल देने के लिए स्व-जीवन दान कर देता है। भट्ठी या अग्नि-कुण्ड में पड़ कर ही स्वर्ण कच्चेपन से निखर कर दिखायी देता है। इसी प्रकार साधुत्व का मूल्य भी नितान्त एकान्त, गुप्त निवास एवं आन्तर संघर्ष के रूप में, जिनके मध्य से साधनारत आत्मा को गुजरना होता है, चुकाना होगा।
आध्यात्मिक पथ घोर तपस्या और शौर्य-युक्त सहनशीलता की अपेक्षा रखता है। ऐसा सामान्य अनुभव उन सभी लगनशील साधकों का है जिन्होंने झूठे और दम्भपूर्ण संसार से पीठ फेर कर आत्म-साक्षात्कार के आदर्श की लौ जगायी है; क्योंकि अन्तिम सत्य है कि मनुष्य और ईश्वर के बीच का सम्बन्ध परीक्षा एवं आपत्तियों की भट्ठी में गढ़ा जाता है।
गुरुदेव कहते थे-'आध्यात्मिकता का कोई शाही (सुगम तथा सुरक्षित) पथ नहीं है। आपदाएँ ही सहनशीलता और इच्छा-शक्ति को, धैर्य और क्षमाशीलता को विकसित करती हैं। अतीत के सभी सिद्धों, सन्तों, भक्तों और योगियों को विपरीत परिस्थितियों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। ईश्वर अपने भक्तों को कठिन परीक्षा में डालता है...।'
ईश्वर द्वारा तुम्हारे धैर्य एवं श्रद्धा की भी परीक्षा होगी। वह तुम्हें पूर्णतया निस्सहाय बना डालेंगे और देखेंगे कि ऐसी विकट परिस्थितियों में तुम्हारे अन्दर उनके प्रति भक्ति है अथवा नहीं। हम नहीं कह सकते, यह परीक्षण किस रूप में होंगे, लेकिन श्रद्धालु भक्त इन परीक्षणों से कभी नहीं डरता।
यदि किसी साधक को अपने परम आदर्श का साक्षात्कार करना है तो सभी विपरीत परिस्थितियों में गम्भीर सहनशीलता और अन्त तक लगे रहने का दृढ़ संकल्प अनिवार्य है; क्योंकि ढालू और सँकरे मार्ग में निश्चय ही कंकरीले-पथरीले रास्ते नीचा प्रयाण होगा।
गुरुदेव ने साधकों के एक समूह को सावधान किया था कि अचेतन आदतों के चुपचाप प्रवेश होने की शक्ति के प्रति सतर्क रहो। 'क्योंकि', उन्होंने कहा था, 'मनुष्य स्वभावतः विलासी है। प्रारम्भ में आप यम-नियम के पालन के प्रति अति-जागरूक होंगे; किन्तु यदि आप सावधान नहीं हैं, तो शनैः-शनैः उत्साह ठण्ढा पड़ जायेगा, विलासिता प्रवेश कर जायेगी और आप बुरी तरह पकड़ में आ जायेंगे। यदि शरीर को विलासिता और सुकुमारता भोगने की पुनः छूट दे दी तो इसको पुनः अनुशासित करना आपके लिए लगभग असम्भव होगा।'
ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जहाँ एकान्तवास करने वाले विरक्त, वर्षों आत्म-संयम के पश्चात् प्रशंसक भक्तों के सम्पर्क में आने से धीरे-धीरे आरामदायक जीवनचर्या में प्रवेश कर गये। जब वे प्रसिद्ध हो जाते हैं, भक्त जन उन्हें घेर कर व्यक्तिगत रूप से सेवा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उत्सुक शिष्यों को निराश न करने की इच्छा से साधक थोड़ी छूट प्रारम्भ में दे देते हैं; किन्तु यह उसके सभी प्रकार के विलासों का गुलाम हो जाने तक बढ़ती ही जाती है।
साधक की कमजोरी के तनिक से संकेत का भी मन तुरन्त लाभ उठाता है। यह एक चीते के समान है जो ताक लगा कर झपटने को ही तैयार बैठा है। स्वामी जी ने अपने जीवन को ही संस्कारों के आकस्मिक आक्रमण के विरुद्ध निरन्तर सदैव सतर्क तथा सावधान रहने का दृष्टान्त बनाया है। वे सबके लिए, यहाँ तक कि स्त्रियों की निकटता से दूर रहने के सम्बन्ध में, ऊँची स्थिति के साधकों के लिए भी, एक आदर्श हैं। भक्त बहुत बार दण्डवत् करते समय उनके चरण-स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे। वे ऐसा करने की कभी छूट नहीं देते थे। नारी-हस्त का स्पर्श वे स्वीकार नहीं करते थे, चाहे वह सच्ची भक्त ही क्यों न हो।
आपने स्वामी विवेकानन्द के सहपाठी के सम्बन्ध में पढ़ा होगा जो एक युवक, त्यागी तथा दृढ़ विचार का साधु था और वर्षों प्रशंसनीय आत्म-संयम तथा निष्काम सेवा के पश्चात् अन्त में एक नारी के कपट-जाल में बुरी तरह फँस गया। साधकों के बीच एक अनौपचारिक वार्तालाप में स्वामी तुरीयानन्द ने यह उदाहरण उद्धृत किया था।
यह पवित्र अथवा अपवित्र होने का प्रश्न नहीं है। विपरीत लिंग के व्यक्तियों का सान्निध्य मात्र ही खतरनाक है। कितना ही पवित्र और सद्भावपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो, नारी के साथ विचरण आदिम शक्ति को छूट दे देता है जो मानव-मात्र के सरल नियन्त्रण के बिलकुल बाहर होता है। महिला स्वयं निष्कलंक हो सकती है, लेकिन भगवान् की बलशाली माया की शक्ति उसके माध्यम से उसके अनजाने कार्य कर सकती है। मनुष्य-हृदय में प्रच्छन्न वासना नारी की उपस्थिति और समीपता में प्रकट होना शुरू हो जाती है। गुरुदेव के समकालीन महान् सन्त येरुपेडु के पूज्य मलयाल स्वामी जो विपरीत लिंग के व्यक्तियों से मिलने-जुलने का दृढ़तापूर्वक निषेध करते हैं, वह अकारण ही नहीं है। उन्होंने एक बार एक साधक से कहा था जिसने अज्ञानतावश एक महिला को, जब वे बीमार थे, अपने स्वास्थ्य के लिए देख-रेख की स्वीकृति दे दी थी और अपने पैरों में दयालुहृदया नर्स से मालिश करायी थी कि 'तुम्हारे इस पतन का प्रायश्चित्त मुझसे बताने को कहा जाये तो मैं महिला द्वारा स्पर्श किये पैरों के हिस्से में दहकते अंगारे लगवाना चाहूँगा।’
एक साधक को नारी के साथ के समस्त सम्पकों का पूर्णतया निषेध करना चाहिए। नारी के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं, उसे प्रशिक्षित तथा उन्नत बना सकते हैं; पर यह सब अलग आश्रम (संस्था) में ही करना चाहिए। उनके लिए विभिन्न आश्रमों की स्थापना की जानी चाहिए और यहाँ तक कि उन्नत महात्माओं को भी उनसे पर्याप्त दूरी से ही सम्पर्क रखना चाहिए।
ब्रह्मा, नारद और विश्वामित्र जैसे मानवेतर व्यक्ति भी किस प्रकार इस काम-प्रभाव के वशीभूत हो गये, इसका हिन्दू-शास्त्रों में विस्तृत वर्णन है। चाहे कोई इन शास्त्रों को आधिकारिक मानने को तैयार हो अथवा न हो; परन्तु शिक्षाएँ जिनसे वे युक्त हैं और जिन्हें वे मनुष्यों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं, महत्त्वपूर्ण हैं। वे आध्यात्मिक साधकों को विपरीत लिंग के साथ सभी प्रकार के सम्पर्कों के परिहार की स्पष्ट शब्दों में वकालत करते हैं। इस तथ्य की अवहेलना से कोई लाभ न होगा कि अधिकांश लोगों में काम-भाव की अधिक तीव्रता होने के कारण ऐसी दुर्द्धर्ष वृत्ति की भूमिका में विवेक और ऐसी दृढ़ शिक्षा (सीख) की अनिवार्य आवश्यकता है।
आध्यात्मिक जीवन चिरकाल के लिए है और साक्षात्कार असीम है। यह अल्पकालिक कार्यकाल की तरह नहीं है जिसके बाद अच्छे विश्राम की अपेक्षा हो। यदि जीवन का कोई भी अर्थ है तो उसी उन्नत, श्रेष्ठ पवित्रता और अनुशासन को बनाये रखना होता है। उत्साह और सतर्कता में कोई भी ढील नहीं दी जा सकती; क्योंकि सांसारिक प्रपंच की प्रबल माया कोई खिलवाड़ नहीं है जो खेली जा सके। वर्षों तक शनैः-शनैः कष्ट-साध्य प्रयत्नों से प्राप्त परिणाम को उड़ाने के लिए वासना का एक झोंका काफी है। इसे स्मरण रखते हुए साधकों को सदैव प्रार्थना के माध्यम से सावधान रहना चाहिए जैसा कि अध्यात्मवादियों ने कहा है।
अच्छा होगा कि हम मदुरै के एक सन्त का उदाहरण स्मरण रखें जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि जब वे उस शहर की सड़कों पर निरुद्देश्य घूम रहे थे, एक अहंकारी एवं उद्दण्ड व्यापारी ने उन्हें सम्बोधित करते हुए परिहास में पूछा, 'इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है-सन्त की ठुड्डी की दाढ़ी अथवा गधे की पूँछ के बालों का गुच्छा ?' सन्त प्रश्नकर्ता को कुछ क्षणों तक मौन देखते रहे और चुपचाप विचरण में लग गये।
कई वर्ष व्यतीत हो गये। एक दिन सन्त ने उस व्यापारी को आवश्यक प्रयोजन हेतु बुला भेजा। मसखरा व्यापारी व्यतीत हुए वर्षों में अपने द्वारा की गयी महात्मा से परिहासमयी मसखरी को भूल जाने के कारण आश्चर्यचकित हो गया कि क्या मामला हो सकता है? उसने पूज्य सन्त को उनकी मृत्यु-शय्या पर देखा और उसके पहुँचते ही मरणासन्न उन्होंने धीरे से उस व्यापारी से फुसफुसा कर इस प्रकार कहा, 'भाई! तुमने कई वर्ष पूर्व मुझसे एक प्रश्न पूछा था। हाँ, मेरी दाढ़ी गधे की पूँछ के बालों के गुच्छे से श्रेष्ठ है। इस प्रकार तुमको तुम्हारा उत्तर मिल गया और मुझे विलम्ब के लिए क्षमा करो।'
व्यापारी ने सन्त से पूछा, 'वर्षों मौन के पश्चात् आपने अशिष्ट प्रश्न का उत्तर अपने अन्तिम क्षणों में अब क्यों देना पसन्द किया?' सन्त ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, 'ठीक कहते हो; क्योंकि ये मेरे अन्तिम क्षण हैं। निःसन्देह, मैंने तभी यह उत्तर दे दिया होता जैसा कि अब दे रहा हूँ, लेकिन मैं साहस न कर सका; क्योंकि मेरे प्यारे भाई, ईश्वर की भ्रामक माया इतनी रहस्यमयी, इतनी अगम्य है कि मैं नहीं जानता था कि अगले क्षण मैं क्या करूँगा अथवा होऊँगा। माया की जादूगरी के सम्मुख मनुष्य के पुरुषार्थ की कोई सामर्थ्य नहीं। दिव्य लीला की रंगस्थली पर वह सर्वोपरि शासक है। कोई भी दृढ़ता से नहीं कह सकता कि वह सभी आकर्षणों से परे है। यह केवल भगवत्कृपा ही है जो मनुष्य को न केवल पवित्र बनाती है, वरन् अन्त तक पवित्र बनाये रखती है। मनुष्य अपनी ओर से केवल सतत विनम्रता एवं सक्रिय सतर्कता रख सकता है। इन सभी वर्षों में मैं अपने को निष्कलंक रखने हेतु प्रयत्नशील तथा सच्चा रहा हूँ। उस परमात्मा के प्रेम और दयालुता पर, पवित्रता बनाये रखने हेत्तु श्रद्धा रखता रहा हूँ। अब मेरे पास जीने के लिए कुछ क्षण ही शेष हैं और फिसलने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपनी अन्तिम श्वास के साथ मैंने आत्मविश्वासयुक्त उत्तर तुम्हें दिया है।' और सन्त पुनः नीचे झुके तथा अपना शरीर त्याग दिया।
अन्धकार से प्रकाश की ओर, असत् से सत् की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाले रपटीले पथ पर अग्रसरित होने के आकांक्षी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह निष्कपट विनम्रता की महान् शिक्षाएँ तथा अविरत सावधानी दृढ़ता से ग्रहण तथा मन में धारण कर ले।
१०. मानवता की सेवा कर दिव्यत्व प्राप्त करें
हे भाग्यशाली मित्र! तुम अज्ञान की प्रगाढ़ निद्रा से कब जागोगे और कब अपने सत्स्वरूप, दिव्य स्वरूप में प्रवेश करोगे ? तुम मात्र यह तन और बुद्धि नहीं हो।
आओ, आओ, अब जाग उठो । अपने जन्मसिद्ध अधिकार की दृढ़तापूर्वक माँग करो। अपने स्वरूप को पहचानो। दिव्य आनन्द, शान्ति और ज्ञान के अनुभव में प्रवेश करो जो कि तुम्हारा अमर स्वरूप है। हे प्रिय मित्र ! ज्योतिर्मय आत्मन् ! इसे अभी करो। तुम निःसन्देह दिव्य हो। तुम अपरिवर्तनशील, असीम तथा अमर आत्मा हो।
जीवन ही साधना है। दिनचर्या ही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मनसा, वाचा, कर्मणा कृत समस्त कार्य ही यज्ञ हैं। यज्ञ अथवा आत्म-त्याग प्रधान सिद्धान्त है और परोपकार इस जीवन का मूल-मन्त्र।
बुद्धिमत्ता और समझदारी से जीवन यापन करो। जीवन का अर्थ और प्रयोजन समझो। अपने वास्तविक स्वरूप तथा अपने यहाँ रहने के कारण को समझो। यहाँ भूलोक में तुम बस एक गुजरते हुए यात्री हो। यहाँ सभी वस्तुएँ क्षणिक हैं। सभी चीजें विनाशशील हैं। अतः अमरत्व को खोजो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भौतिक नहीं है। यह आध्यात्मिक और मृत्युरहित है। अपने सत्स्वरूप का, अपने अमर रूप का साक्षात्कार करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम इस साक्षात्कार हेतु परिश्रम से प्रयास कर रहे हो तो अपने चतुर्दिक् के संसार में आदर्श सम्बन्ध स्थापित करो। सभी लोगों के प्रति महानता, सहानुभूति, दयालुता, प्रेम, निःस्वार्थता तथा सेवा की दृढ़ इच्छा से सम्बद्ध बनो।
मानवता की सेवा कर दिव्यत्व प्राप्त करो। सभी प्राणियों के प्रति करुणा ही परमानन्द की कुंजी है। विनम्रता सर्वोच्च गुण है। सत्यता सम्पत्ति का विशालतम कोष है। आत्म-संयम सर्वोत्कृष्ट प्राप्तव्य पूँजी है। अज्ञानता निकृष्टतम दोष (कलंक) है। अतः यह पूर्णतया उन्मूलन योग्य है।
एक आदर्श व्यक्ति बनो। आध्यात्मिकता से प्रकाशित आत्मा बनो। इस प्रकार जीवन को ज्ञान, शान्ति और आनन्द से सराबोर बनाओ। तब तुम समस्त मानवता के लिए आनन्दप्रदाता (कल्याणकारी) बनोगे। मैं तुम्हारे सुख और शान्ति की कामना करता हूँ!
११. तृतीय कपालवत् बनो
हम प्रातः-सायं ध्यान अवश्य करते हैं; किन्तु दिन में अपने कार्य-कलापों में और अन्य व्यक्तियों से व्यवहार करते समय हम तुच्छ विचार और स्वार्थ प्रदर्शित करते हैं। यह हमारी साधना को अवरुद्ध करता और ध्यान के लाभों को निरर्थक बना डालता है। यूलीसस की पत्नी पेनीलोप के अपने पति की अनुपस्थिति में बहुत से विवाह-प्रार्थी थे जिनके साथ वह कभी विवाह करना नहीं चाहती थी; क्योंकि वह पति-परायणा और पतिव्रता स्त्री थी। अतः उनको धोखा देने और समय व्यतीत करने के लिए उसने एक चाल खोज निकाली। उसने अपने विवाह-प्रार्थियों से कहा कि वह स्वेटर तैयार कर रही है और जब तक स्वेटर पूरा बुन नहीं जाता, वह किसी को भी स्वीकार नहीं करेगी। वे राजी हो गये। यूलीसस के आने तक वह प्रतिदिन दिन में स्वेटर को बुनती और रात को बुने हुए को उधेड़ डालती रही। किये-कराये को पुनः न करने का यह एक अच्छा उदाहरण है।
हमें इस प्रकार के 'विनाश' को अपनी साधना में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। ब्राह्ममुहूर्त काल में हमने जो अच्छा अभ्यास किया हो, हमें उसमें आसुरी तत्त्व नहीं संयुक्त करना चाहिए।
यदि अपने क्रिया-कलाप के बीच हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, रूखे तथा बेईमान हो जाते हैं और अन्य व्यक्तियों की आलोचना प्रारम्भ कर देते हैं, तो यह सब प्रातः ध्यानकालीन जो साधना है, उसको व्यर्थ कर देंगे। अतः हम क्षणभंगुर भौतिक जीवन और कर्म, वाणी तथा क्रियाओं पर सजग चौकसी रखें और ध्यान, पूजा एवं साधना की धारा को प्रगतिशील बनाये रहें।
अतः यह अति आवश्यक है कि हम अपनी साधना को पूजा-कक्ष के अन्दर शान्त प्रहरों तक ही सीमित न रखें, बल्कि अपनी समस्त क्रियाओं को दिव्यता में ढाल लें। हमें अपने समस्त कार्यों को, अपने सत्स्वरूप को प्रकटित करना चाहिए। उनको आध्यात्मिकतामय हो जाना चाहिए। यह समस्त क्रियाओं का दिव्यीकरण ही 'कर्मयोग' कहा जाता है।
जो मनुष्य आत्म-त्याग से पूर्ण, मधुरता एवं सहयोग से पूर्ण एक आदर्श जीवन व्यतीत करता है, एकमात्र वह व्यक्ति ही अपनी साधना को प्रभावपूर्ण और सफल बनाता है।
अतः साधक को विवेकी होना चाहिए। सक्रिय जीवनचर्या के साथ उसे अपनी साधना में विरोधाभास नहीं लाना चाहिए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि पात्र कहाँ चू रहा है, अन्यथा पात्र भरते रहना व्यर्थ है।
एक साधक को सावधान, सजग, चुस्त और सूक्ष्म बुद्धि वाला होना चाहिए। तीन कपालों की कथा स्मरण-योग्य है।
एक बार एक राक्षस एक राजा के दरबार में तीन कपालों के साथ आया और राजा को धमकाया कि यदि सही तौर से निर्दिष्ट न कर सका कि इन तीनों में कौन कपाल श्रेष्ठ है तो वह उसे खा जायेगा। राजा ने तीन दिवस का समय माँगा और राक्षस ने स्वीकृति दे दी। तब राजा ने अपनी राजसभा में विद्वानों से पूछा, 'उन तीनों में कौन कपाल श्रेष्ठ है?' कोई कुछ भी न कह सका; क्योंकि बाह्यतः तीनों पूरी तरह मिलते-जुलते थे।
एक बुद्धिमान् पण्डित आया और प्रथम कपाल के एक कान के बीच से सलाख डाल दी जो सीधे दूसरे कान के बीच तक चली गयी।
तब उसने द्वितीय कपाल के मध्य से सलाख प्रवेश करायी। इस बार एक कान के मध्य से डाली गयी सलाख मुख से बाहर आ गयी।
तब सलाख तृतीय कपाल के मध्य से प्रवेश करायी गयी। इस बार एक कान के मध्य से डाली गयी तो वह सीधे हृदय में चली गयी। राजसभा के पण्डित ने निरूपित किया कि तीसरा कपाल सर्वश्रेष्ठ है।
प्रथम कपाल उस कोटि के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान को एक कान से सुनते हैं और बिना अभ्यास किये दूसरे कान से निकाल देते हैं और उसको विस्मरण कर जाते हैं। द्वितीय कपाल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् दूसरों को उपदेश देने को तो उत्सुक रहते हैं; किन्तु स्वयं उस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते। यह द्वितीय श्रेणी के लोग हैं।
तृतीय कपाल सर्वश्रेष्ठ कोटि के साधकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान को श्रवण के पश्चात् अपने हृदय में स्थित कर लेते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं। अतः आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि तृतीय कपालवत् बनो। ज्ञानियों, सन्तों और महात्माओं के सत्संग से जो-कुछ भी सीख सको, उसका पोषण एवं अभ्यास करते रहो। परमेश्वर का तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो!
१२. सरल, निष्कपट, विनम्र एवं सहनशील बनो
सभी सन्तों और पुण्यात्माओं ने अपने स्वयं के उज्ज्वल उदाहरण द्वारा भौतिक बन्धनग्रस्त आत्माओं के अज्ञान की तिमिर रजनी को राकेश के समान ज्योतित किया है।
वे कुटिलता एवं धूर्तता से रहित अतीव सरल स्वभाव के मनुष्य थे। सभी प्रभुभक्तों में सरलता और निष्कपटता ही उनकी विशेषताएँ थीं।
'जब तक तुम छोटे शिशुओं के समान नहीं बनते, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते।' यह ईसामसीह की रहस्यमयी घोषणा है।
सभी सच्चे महान् सन्त किसी व्यक्ति पर अविश्वास करना नहीं जानते। उन्होंने सभी पर विश्वास किया। यह उनके चरित्र का सबसे मुख्य विशिष्ट गुण था। वे निष्कपट थे। उनमें तथाकथित धूर्तता तथा चतुराई न थी जैसी कि संसारी मनुष्यों में रहती है और उसे अपनी प्रगति हेतु आवश्यक समझते हैं। किन्तु आगे कहाँ बढ़ना है? यह सर्वथा एक अलग प्रश्न है। प्रश्न यह है कि यह सही दिशा-स्वर्ग तक बढ़ने जैसा है अथवा अपने विनाश की ओर अर्थात् अपने अधःपतन की ओर बढ़ना है? तथाकथित धूर्तता, जो कि मनुष्य अपनी प्रगति हेतु आवश्यक समझता है, सन्तों में उसका अभाव था, पर वे इस हेतु घाटे में नहीं थे। वे पूजनीय हो गये। वे अमर हो गये; क्योंकि वे निष्कपट थे। उनका स्वभाव पवित्र और सरल, स्फटिक-सा निर्मल था और यही शिशुओं का स्वभाव है। सन्त बच्चों के समान थे। शिशु जैसी सरलता, शिशु जैसी निष्कपटता, शिशु जैसा भोलापन, स्फटिक जैसी हृदय की पवित्रता सदैव से सन्तों के सामान्य लक्षण रहे हैं।
दूसरी बात है विश्वव्यापी लक्षण 'अहंकार' जो सहस्र में नौ सौ निनानवे मनुष्यों में पाया जाता है। लोग अहंकारी हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के अहकार से युक्त है। मनुष्य सोचता है, 'मैं कुछ हूँ' और वह उपेक्षित नहीं होना चाहता। वह दूसरों द्वारा स्वयं को विशिष्ट रूप से समझे जाने की आकाक्षा करता है और अपने-आपको प्रदर्शित करना चाहता है। यह अहकार तत्त्व-किसी से अपने-आपको श्रेष्ठ समझने की भावना सन्तों में नहीं होती। वे विनम्र थे। वे विनम्रात्मा थे। वे निरहंकारी आत्मा थे।
'भाग्यहीन हैं वे जो आत्मवृत्ति में दर्पहीन हैं; क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।' दर्पहीन धन की दृष्टि से नहीं। वह सभी वस्तुओं का स्वामी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह अनुभव करता है कि भगवान् के चरणों में वह धूल का एक कण है। परमेश्वर ही सब-कुछ है। मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे भगवान्! आप ही सब-कुछ हैं। सभी पवित्रात्माओं का यही दृष्टिकोण है और यह पूर्ण अहंकारशून्यता तथा उससे उत्पन्न विनम्रता भी समस्त सन्तों की सार्वलौकिक चारित्रिक विशेषताएँ हैं।
जैसे अहंकार साधारण मनुष्यों के विकासहीन दिनों की विश्वव्यापी विशेषता है-उन मनुष्यों की जो माया के चंगुल में हैं-ठीक उसी प्रकार सभी सन्तों की विश्वव्यापी विशेषता रही है 'पूर्ण विनम्रता'। भाग्यवान् हैं वे जो विनम्र हैं। और उसी पंक्ति का भाव प्रतिध्वनित हुआ था भारत में जन्मे एक श्रेष्ठ सन्त द्वारा। वह चैतन्य महाप्रभु थे। वे कहते हैं, 'त्रिणादपि सुनीचेन'- (साधक को) अपने-आपको घास के तिनके से भी निम्न समझना चाहिए।
अहंकारी मनुष्य ने अब तक इस रहस्य को, इस सत्य को नहीं समझा है कि अहंकार मनुष्य के वास्तविक शिष्ट संस्कार और प्रगति में महान् अवरोध है। वह तर्क देता है कि यदि मनुष्य अपने-आपको 'कुछ' नहीं समझता है तो वह कुछ भी प्राप्त न कर सकेगा और इस प्रकार अत्यधिक विनम्रता व्यक्ति का केवल जीवन ही नष्ट करती है।
लेकिन सन्तों ने इससे अच्छा जाना है। उन्होंने जाना कि संसार में क्या निष्पादन योग्य है और वास्तव में सम्यक् निष्पादन क्या है और उन्होंने जाना कि अहंकार चिरस्थायी मूल्य के अच्छे पदार्थों के पाने में महानतम अवरोध है और इसलिए वे विनम्र, सहनशील और क्षमावान् थे। सन्तों के जीवन परीक्षा और क्लेशों से पूर्ण थे। उनको क्लेश दिये गये। उनको अत्यधिक कठिनाइयों को सहन करना पड़ा। परमेश्वर ने उन्हें कठिनाइयों और क्लेशों, कष्टों और यातनाओं की भट्ठी में डाला।
जैसे कि स्वर्ण को समस्त मल से शुद्ध होने तथा शुद्ध धातु के रूप में चमकने के लिए भट्ठी में डाला (तपाया) जाता है, उसी प्रकार सन्तों को भीषण क्लेश और कष्ट में डाल दिया गया और इन सबके मध्य से उन्होंने तीन विशिष्ट गुण स्पष्ट प्रकटित किये :
प्रथम था कि उन्होंने समस्त परीक्षाओं और क्लेशों को ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया और उनको सहन किया। सहनशीलता, धैर्य, क्षमा-ये सन्तों के लक्षण सदैव रहे हैं और सदैव रहेंगे।
हे मनुष्य! सहन कर।
ईसा का उदाहरण, जो चरम सीमा तक गया है, महान् शिक्षादायक है कि मनुष्य को चुपचाप पीड़ा एवं कष्टों को सहन करना है और केवल इसी सहनशीलता एवं कष्टों के मध्य से वह मलरहित शुद्ध स्वर्ण रूप निखरता है।
जीवन के समस्त वेदनापूर्ण एवं उलट-फेर के अनुभवों को चुपचाप सहन करने की प्रक्रिया में उन्होंने कभी विश्वास नहीं खोया; बल्कि जितना अधिक उन्होंने सहा, उतना अधिक ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली तथा उनकी श्रद्धा और अधिक शक्तिशाली व दृढ़ हो गयी। यह उनमें दूसरा विशेष गुण था। 'हे परमात्मन्! आप घोर-से-घोर क्लेश भेज सकते हैं; किन्तु मैं आपमें श्रद्धा नहीं छोड़ सकता, हे ईश्वर!' यह था आश्चर्यजनक उत्साह जो वे रखते थे। उन्होंने कभी ईश्वर पर से श्रद्धा नहीं छोड़ी। तीसरा गुण था कि उन्होंने अपने को हानि पहुँचाने वालों को न केवल क्षमा किया, बल्कि उनके लिए समस्त हित की कामनाएँ भी की। हे साधक! ऐसी सहनशीलता रखो और विनम्र बनो। तुम्हारे ऊपर कुछ भी घटित हो, पर कभी श्रद्धा न छोड़ो और निश्चय ही तुम्हें अमर जीवन तथा असीम आनन्द का पारितोषिक मिलेगा।
१३. उनके चरण-चिह्नों का अनुसरण करो
जो सन्तों पर मुसीबत ढाने में कारण-रूप थे, उन सभी के प्रति सन्तों का दृष्टिकोण क्षमा और बुराई का बदला अच्छाई से चुकाने का था। जिन लोगों ने उनको अधिकतम हानि पहुँचायी, उनका हित करने का उन्होंने प्रयत्न किया। प्रत्येक स्थिति को सहन करना, सदैव ईश्वर में अपनी दृढ़ और अडिग श्रद्धा एवं सतत क्षमावान्-यही सन्तों का स्वभाव है और यही विशेषताएँ समस्त विश्व के सन्तों में पायी जाती है। सभी लोग जो आध्यात्मिकता में उन्नत तथा मानव मात्र से पूज्य हुए हैं, उन्होंने सदैव इन आश्चर्यजनक गुणों को प्रकट किया है। सन्तों के लिए ईश्वर सुदूर की कोई सत्ता नहीं है, प्रत्युत् सदैव जीवन्त वास्तविकता है। जैसे हम एक-दूसरे के लिए उपस्थित हैं, उनके लिए भी ईश्वर सदैव वर्तमान है। जीवन के प्रत्येक क्षण में वे 'उसकी' ओर उन्मुख होते हैं। जब कभी उन्हें सहायता, सान्त्वना, शक्ति, मार्गदर्शन या प्रकाश की आवश्यकता होती तो वे तुरन्त बिलकुल वैसे ही ईश्वरोन्मुख हो जाते थे जैसे बच्चा अपने माता-पिता की ओर उन्मुख होता है। परमात्मा उनके सम्मुख सदैव उपस्थित थे और इस प्रकार उनके जीवन 'पराशक्ति' की उपस्थिति की जानकारी से सदैव रूपान्तरित रहे जिसको कि वे अपना निजी सत्त्व अनुभव करते थे। वे अपने और ईश्वर के बीच समस्त भेद विगलित कर चुके थे। वे अपने-आपको ईश्वर के अति-घनिष्ठ अनुभव करते थे। वे ईश्वर को अपना ही अनुभव करते थे।
हम भी ईश्वर के साथ प्रतिदिन यह घनिष्ठता अपनी प्रार्थना, स्तुति द्वारा व्यक्त करते हैं; किन्तु हम काफी गहराई से अनुभव नहीं करते। आपत्तियों के समय हम अपने अन्तर्वासी के बजाय अपने धन या अन्य बाह्य सांसारिक साधनों पर अधिक निर्भर करते हैं। ईश्वर है, इसकी भावना हमारे में नहीं है।
परन्तु सन्त, जब वे बाह्य विश्व में भी रह रहे होते हैं तब भी सदा ईश्वर के निकटतम सम्पर्क में रहते हैं। इसलिए वे भागवत पुरुष हैं। वे ईश्वरमय जीवन यापन करते हैं और सदैव ईश्वर को ही वास्तविक सम्पत्ति, सर्वोत्कृष्ट धन, जीवन में पाने योग्य एकमात्र वस्तु मानते हैं। वे अन्य कोई इच्छा कभी नहीं रखते। उनकी निष्कामता अन्ततोगत्वा ईश्वर में विश्राम लेती है और उनके हृदय को सन्तोष से परिपूर्ण कर देती है।
सभी सन्त जाति-पाँति से ऊपर उठे हुए हैं। वे एक परिवार-ईश्वर का 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के थे। पूर्ण पवित्रता, ईश्वर में पूर्ण विश्वास, करुणा, सन्तोष, कामनाराहित्य, पूर्ण निष्कपट स्वभाव और केवल ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता-ये गुण तुम सभी सन्तों में पाओगे।
पश्चिमी देशों के सन्तों में किसी एक का उदाहरण लो। तुम उनमें वही सरलता, वही विनम्रता, वही स्पष्टवादिता पाओगे। यहाँ तक कि यदि कोई मनुष्य उनका गला ही काटने वाला था, उन्होंने उसको भी गले लगाया। यह सन्तत्व की प्रतिक्रिया थी। वे इस दैवी गुण की भावना से ओत-प्रोत थे। संक्षेप में उन्होंने 'अमृताष्टक' (श्रीमद्भगवद्गीता के बारहवें अध्याय के अन्तिम आठ श्लोकों) की भावना को क्रियान्वित किया है जिसमें श्रीकृष्ण भगवद्-भक्त, जो कि भगवान् को भी प्रिय है, के लक्षणों का वर्णन करते हैं।
हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि इन सन्तों के अन्तस्तल की छानबीन करें और वैसा ही अनुभव करें जैसा कि उन्होंने अपने हृदयों में अनुभव किया था-ईश्वरार्थ उमड़ता हुआ प्रेम, क्षमाशीलता, मातृवत् करुणा, गम्भीर श्रद्धा ही ऐसे भाव थे जिन्होंने उनके पथ में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को झेलने की क्षमता प्रदान की थी। उन्होंने हिमालय के समान अध्यवसाय एवं धैर्य ईश्वर-साक्षात्कार के पथ पर चलते हुए प्रदर्शित किया।
यदि अपने खुले हृदय से पक्षपात-रहित हो, हम उन सन्तों के स्वभाव में गहरी खोज करें तो उनके व्यक्तित्व के सभी श्रेष्ठ विशिष्ट गुण हमारे सम्मुख आ जायेंगे और उन महान् गुणों को हम अपने हृदय में उसी रूप में अंकित कर सकेंगे तथा उनके समान बन सकेंगे। निस्सन्देह ! केवल यह ही एक प्रभावशाली पद्धति होगी जिससे इन महान् आत्माओं की हम पूजा कर सकते हैं, जिससे उनकी शिक्षाओं का हम श्रद्धा और सम्मान की भावना के साथ पालन कर सकते हैं तथा उनके सारगर्भित आदर्शों एवं चारित्रिक विशेषताओं को आत्मसात् करने का प्रयत्न कर सकते हैं।
यह प्रतिस्पर्धा एक महानतम श्रद्धांजलि होगी, जो इन सन्तों को हम अर्पित कर सकते हैं।
हमें उनको अपने में आत्मसात् करने की स्पर्धा करनी चाहिए। अपने जीवन के उदाहरण द्वारा उन्होंने जो महान् आदर्श हमारे सम्मुख उपस्थित किये हैं, हमें उनके अनुसरण का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए दिव्य जीवन के आदर्श, जो कि उन्होंने प्रस्तुत किये हैं, उनका दृढ़तापूर्वक हम अपने को अनुगामी बनायें। इन महान् आदर्श पुरुषों-जैसा हम अपने-आपको श्रद्धापूर्वक रूपान्तरित करें तो यह सर्वोच्च प्रभावशाली पद्धति होगी जिसके द्वारा इन सन्तों को हम अपनी श्रद्धांजलि और सम्मान अर्पित कर सकते हैं।
१४. भक्त सुरक्षित होता है
ऐसा मानना एक सामान्य भ्रम है कि जो भक्ति-मार्ग के लोग हैं, जो श्रद्धा का विकास करते हैं, जो प्रार्थना, शरणागति और भगवन्नाम का आश्रय लेते हैं, क्लीववत् निर्बल हो जाते हैं और वे वेदान्तियों के समान सुदृढ़ नहीं होते। वेदान्ती सदैव बलशाली होते हैं, वे वनराज सिंह का रूप प्रस्तुत करते हैं जो किंचिन्मात्र नहीं डरता और शक्ति-सम्पन्न होता है। उसी भाँति वेदान्त-केसरी से केसरी जैसी गर्जना की कल्पना की जाती है।
वास्तविक भक्त भी वेदान्ती के समान ही होता है। वह इस विश्व में किसी से भी नहीं डरता। उसकी शक्ति अपरिमित होती है; क्योंकि उसकी शक्ति अकेले एक व्यक्ति की शक्ति नहीं होती। उसकी शक्ति का स्रोत अनन्त होता है जिसमें कि वह अपने-आपको संस्थित कर चुका होता है। शक्ति-स्रोत वेदान्ती और भक्त के लिए एक वही है। वेदान्ती आत्मा पर भरोसा करता है, किन्तु भक्त भगवान् पर भरोसा करता है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म एक हैं। इसलिए यदि एक भक्त अपने अन्दर किसी प्रकार का भय या निर्बलता का अनुभव करता है तो उसका तात्पर्य हुआ कि उसकी भक्ति की साधना समुचित नहीं है। उसमें कुछ कमी है। वहाँ कुछ त्रुटि है। यदि वह वास्तविक भक्त है, उसको पूर्णतया निर्भय होना चाहिए। उसे कहना चाहिए, 'मेरे अधरों पर भगवन्नाम है। समस्त विश्व में भगवन्नाम की तुलना में कुछ नहीं। अतः मुझको संसार से कोई भी भय नहीं आ सकता।' इस प्रकार वास्तविक भक्त किसी से नहीं डरता। इस प्रकार वास्तविक भक्त किसी से नहीं डरता। माया उसका कुछ भी नहीं कर सकती। जो अपने अधरों पर सदैव भगवन्नाम रखता है, वह माया के छल-प्रपंच को चुनौती देता है। जिसने भगवन्नाम में श्रद्धा और भक्ति रखे हैं, उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। उसकी सुरक्षा पर आँच नहीं आ सकती। उस पर कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वह श्रद्धा पर निर्भर करता है।
ऐसी ही श्रद्धा हनुमान् जी में थी जिनका यशस्वी व्यक्तित्व रामायण के पृष्ठों में हमारे सम्मुख जाज्वल्यमान् है। वे सच्चे भक्त के आदर्श हैं-भक्त जो कि शक्ति-सम्पन्न है, साहस से पूर्ण है, शौर्य से पूर्ण है। सच्ची भक्ति से बल आता है। वास्तविक प्रेम असीम साहस और निर्भयता प्रदाता है।
माया को जीतने के संग्राम में साधक को पोषित करने वाली समस्त शक्ति का स्रोत क्या है? भगवन्नाम ही बल है। वह बल है, सच्चे प्रेम और भगवद्-भक्ति का बल। वह बल है भगवान् में पूर्ण श्रद्धा, भगवद्-कृपा में श्रद्धा और उसके नाम में श्रद्धा का बल; उदाहरणार्थ हनुमान् जी का यशस्वी नाम हमारे सम्मुख आदर्श रूप में प्रस्तुत है।
एक भक्त किसी से भय नहीं करता। कोई बाधा उसे उस मार्ग पर आरूढ़ होने से विचलित नहीं कर सकती जो भगवत्-मिलन की ओर ले जाता है। यदि ऐसी वास्तविक भक्ति नहीं है तो भीरुता और इसी प्रकार की अन्य बातें आ जाती है।
१५. हनुमान् और रावण में विरोधाभास
हनुमान् जी की अपरिमित शक्ति का रहस्य क्या था? वे एक छलाँग में कैसे सागर पार कर सके ?
इसलिए क्योंकि वह दिव्य नाम के अनन्य उपासक थे। यह भक्ति ही थी जिसने राक्षसों पर विजय पाने की उन्हें असीम शक्ति प्रदान की। हनुमान् जी के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता था। वे अपने शौर्य में अद्वितीय थे।
उनमें असीम बल था, किन्तु तब वे रामायण के एक अन्य व्यक्तित्व से अद्भुत रूप से भिन्न दिखते हैं। वह था रावण का व्यक्तित्व जिसका बल भी असीम था, जिसके बल के सम्मुख त्रिलोक काँपता था-ऐसा व्यक्ति जिसने कैलास पर्वत उठा लिया, जिसने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की और अग्निदेव को अपना रसोइया बनाया, वरुणदेव को अपने उद्यान का भिश्ती बनाया और समस्त अष्टदिग्पालों को अपना दास बनाया। नवग्रह उसके सिंहासन की सीढ़ियाँ थे। ऐसा रावण का महाबल था। लेकिन तब रावण ने क्या किया ? यह रावण का महाबल, यह महान् शक्ति जो कि किसी अन्य ने नहीं स्वयं भगवान् विष्णु के अवतार ने वशीभूत कर ली, अहंकार ने बरबाद और नष्ट कर दी। यह शक्ति अधर्म से भी संयुक्त थी। अहंकार और अधर्म ने पूर्णतया रावण की इस महान् शक्ति को दूषित और विकृत कर दिया और एक आश्चर्यजनक भिन्न रूप में हमारे सम्मुख एक महान् व्यक्तित्व हनुमान् जी का, जो कि अपनी ऊँचाई में शिखरवत् है, किन्तु फिर भी आश्चर्यजनक, अत्यधिक सुन्दर, पूर्ण विनम्रता और आत्मलोप का उदाहरण है; आता है। हम सदैव हाथ जोड़े हनुमान् जी का चित्र देखते हैं।
यत्र-यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र-तत्र कृतमस्तकांजलिम्।
वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ।।
समस्त बल, साहस, शौर्य और अन्य दिव्य गुणों से युक्त अतुलनीय विनम्र हनुमान् जी का ऐसा हृदय था जो प्रेमाश्श्रु में सदैव द्रवित हुआ करता था और जो सदैव सेवापरायण एवं विनम्रतापूर्ण था। यह मानवता के दोनों पक्षों के लिए एक प्रत्यक्ष शिक्षा का पाठ है। दोनों रूप में राष्ट्रों के रूप में, व्यक्तिगत रूप में-किस-किस प्रकार उन्हें पूर्ण क्षमताओं, योग्यताओं और शक्ति को भगवान् की सेवा में उपयोगी होना चाहिए। शक्ति और क्षमता को कैसे पूर्ण विनम्रता से सम्पन्न करना चाहिए। यह सबसे बड़े महत्त्व का पाठ है जो हनुमान् जी का व्यक्तित्व मानव मात्र को सदा सिखाता है। यदि यह भाव हममें नहीं है तो हम स्वयं को रावण-सा पायेंगे और हमारा पतन अवश्यम्भावी है।
हनुमान् जी का नाम अमर हो गया; क्योंकि उनका अपरिमित बल अतुल विनम्रता से संयुक्त था-विनम्रता इतनी गहरी और विस्तृत जैसा सागर; और आज्ञाकारिता एवं सेवा की पूर्ण भावना। हनुमान् जी सदैव भगवान् के सेवक हैं। हाथ जोड़े और शरणागत भाव से भगवान् की कुछ सेवा करने का कोई सुअवसर पाने की प्रतीक्षा में रत हैं। वे पूर्णरूपेण भक्त, पूर्णरूपेण दास और सेवक थे और आध्यात्मिक साधक थे। उन्होंने अपने अहंकार का दमन कर रखा था। उनका मस्तक कभी आप उठा हुआ नहीं पायेंगे। वे सदैव उसे नीचे झुकाये रखते हैं। इसलिए भगवान् राम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। जब पट्टाभिषेक का समय आया, श्रीराम ने हनुमान् जी को अपने सम्मुख स्थान दिया। यह उस पूर्ण भक्ति, विनम्रता, सेवा-भाव, पूर्ण अहं-शून्यता एवं पूर्ण आत्मलीनता का पारितोषिक था।
एक बार हनुमान् जी से प्रश्न किया गया, 'आज सप्ताह का कौन-सा दिन है और कौन-सा ग्रह तथा तिथि है?' इस पर उन्होंने उत्तर दिया, 'न मैं दिन जानता हूँ न ग्रह। मैं केवल श्रीराम को, उनके नाम को और उनके प्रेम को जानता हूँ।'
उनके जीवन का उद्देश्य केवल श्रीराम का प्रेम था और ऐसे प्रेम का परिणाम है कि श्रीराम सदा उन्हें अपने सामने रखते हैं। यह अन्यतम पद उन्हें प्राप्त हुआ। हनुमान् जी के बिना श्रीराम नहीं हैं।
वे एक आदर्श साधक हैं जो आदर्श विनम्रता, पूर्ण शरणागति और आज्ञाकारिता के गुणों से युक्त हैं। यदि आप हनुमान जी के सम्पूर्ण जीवन का विश्लेषण करें तो यह निरन्तर और अन्त तक भगवान् की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हनुमान् जी के व्यक्तित्व का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश जो हमें स्मरण करना चाहिए, वह है राम-प्रेम और उनकी विनम्रता जिसने उन्हें अमर बना दिया। अतएव बल (पुरुषार्थ) जब भगवद्-भक्ति और भगवद्-पूजा से संयुक्त हो तो उसकी निष्पत्ति अमर महिमा में तथा ईश्वर के शाश्वत मिलन में होती है।
जो व्यक्ति गुण, भक्ति, विनम्रता, सेवा-भावना और पूर्ण शरणागति जैसी अपने शरीर और मन की समस्त क्षमता को भगवान् से संयुक्त कर देता है, उसे सर्वोच्च उपलब्धि होती है। भगवान् का नाम सदा दोहराते रहने में लवलीन रहना और भगवद्-सेवा में सदैव संलग्न रहना, यह एक भक्त का ज्वलन्त आदर्श है। हनुमान् जी का महान् व्यक्तित्व इस आदर्श को मानवता के सम्मुख सदैव प्रस्तुत करता है।
हमारे लिए, आध्यात्मिक साधकों के लिए, साथ-ही-साथ इस विश्व के मानव मात्र के लिए अपने बल को धर्म से संयुक्त करना और इस प्रकार भगवान् से सनातन एकता प्राप्त करना-ऐसी उनके व्यक्तित्व की यशः प्रशस्ति है और ऐसी इस आदर्श व्यक्तित्व की महत्ता है।
१६. एक साधु के नियत कर्तव्य
इस भूलोक के लोगों को तीन बृहत् श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के लोग केवल इसी भूलोक के जीवन पर विश्वास करते हैं। द्वितीय श्रेणी ऐसे लोगों की है जो कुछ सेवा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विहीन हैं। तृतीय श्रेणी के लोग हैं जिनमें जिज्ञासा जागरूक है, जिनमें श्रेष्ठतर क्षीर-नीर-विवेक क्रियाशील है, जो जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखते कि यह कुछ काल का, यहीं समाप्त हो जाने वाला है। आगे का वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है और इसलिए उसकी कोई चिन्ता नहीं करते। वे इस जीवन को एक सुअवसर मानते हैं जो इस जीवन का अतिक्रमण कर महत्तर को उपलब्ध करने को दिया गया है। इन साधकों को यह भी ज्ञात है कि तत्त्वतः वे भौतिक नहीं हैं और उनका जीवन इस भौतिक (स्थूल) जीवन के साथ ही समाप्त नहीं होता। उन्हें ऐसा आभास होता है कि उनका जीवन वास्तव में आत्म-बोध की दृष्टि से सनातन अस्तित्व है तथा शान्ति, आनन्द एवं ज्ञान स्वरूप है। वे सोचते हैं कि उनका भौतिक जीवन एक अस्थायी बन्धन है।
वे अपने वास्तविक जीवन का जो कि उनका असली जीवन है, उसका अनुभव पुनः प्राप्त कर लेने को उत्कण्ठित हैं। अतएव वे इस वर्तमान भौतिक सत्ता का प्रयोग अज्ञानावस्था को पार करने हेतु दृढ़-निश्चयी संघर्ष में लगाते हैं जिससे कि वे उस महा-अनुभव को, आत्मिक जीवन को पुनः प्राप्त कर लें। ऐसे लोग साधक तथा जिज्ञासु के रूप में जाने जाते हैं।
इस श्रेणी के लोगों को जो आध्यामिक आदर्श हेतु जीवन यापन कर रहे हैं, सम्पर्क में लाने और उनको प्रेरणा देने एवं उनको आध्यात्मिक लक्ष्य के समीप पहुँचाने के लिए ही श्री गुरुदेव जैसे आत्मसाक्षात्कार-प्राप्त पुरुषों ने दिव्य जीवन संघ जैसी संस्थाएँ स्थापित की हैं। साधु संघ एक समधिक उद्देश्य को ले कर प्रारम्भ किया गया था अर्थात् विभिन्न भक्तों के रूप में समस्त शक्ति को एकत्रित करना जिससे कि समस्त सन्तों के मध्य एक ऐक्य स्थापित किया जा सके, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं तथा साधकों में एक प्रकार का विश्व-बन्धुत्व लाया जा सके। यह विचार प्रचलित है कि साधु का अर्थ है गेरुआ पोशाक पहने हुए संन्यासी। स्वामी जी इनको नकारते थे। साधु या संन्यासी वह है जिसमें आध्यात्मिक आदर्श ही केवल मात्र आदर्श है, वह चाहे गृहस्थ हो या त्यागी हो।
किस पद्धति से हम साधु-जीवन-दिव्यता का खोजपूर्ण जीवन-का प्रचार करने योग्य होंगे और क्रियात्मक रूप से हम अपने जीवन के क्षेत्र में अधिक-से-अधिक लोगों में भगवद्-साक्षात्कार वाले इस श्रेष्ठतम जीवन के प्रति जागरण लाने के लिए क्या कर सकते हैं? संसार के सामान्य मनुष्य से साधु एक पूर्णतः विपरीत श्रेणी के होते हैं। यदि संसारी मनुष्य किसी वस्तु को वांछनीय मानता है तो साधक इसको धूल से भी हीन मानता है। संसारी मनुष्य के लिए जो वस्तु आनन्ददायक है, साधक के लिए वही अत्यधिक कष्टदायक है। संसारी मनुष्य जिसको जीवन के लिए आवश्यक मानता है, साधक वास्तविक प्रगति में उसे महान् विघ्न मानता है। यहाँ तक कि ऐसी प्रगति सम्बन्धी दृष्टिकोण में भी दोनों एक-दूसरे के पूर्णतया विपरीत होते हैं। यदि यह सत्य है तो साधु को संसार में अनुपयुक्त (Misfit) होना ही चाहिए और किसी सीमा तक यह सत्य भी है; लेकिन वास्तविक साधु पूर्णतः अनुपयुक्त नहीं होता। साधुओं का समाज संसार में अल्प संख्या में है। साधु में परिस्थिति अनुसार अपने को ढालने की अत्यधिक क्षमता होती है। वह जानता है कि जब ईश्वर विश्व को सहन करता है तब वह भी संसार को सहन करने को तैयार है।
साधु अनिवार्यतः सार्वलौकिक होता है। यद्यपि वह संसार को दुःखी हृदय से देखता है; पर वह बहुत सहनशील होता है। वह अन्यों के साथ उनके अनुकूल हो जाता है, किन्तु अपने स्वयं के आदर्शों में दृढ़ निश्चयीही होता है।
श्री स्वामी जी को देखिए-उनमें इस सत्य का जीता-जागता उदाहरण पायेंगे। कभी-कभी राजनीतिज्ञ आ कर अपने दृष्टिकोणों को हवा में उछालते और अपनी समस्याओं को उनके सम्मुख रखते हैं। वे धैर्यपूर्वक नि उनको सुनते हैं और इस प्रकार परामर्श देते हैं मानो वह उन समस्याओं में बहुत ही रुचि रखते हों, जब कि वे सभी समय उस आत्म-चेतना में रहते हैं। जो अनुभूति कराती है कि यह केवल मात्र धुएँ के गुबार सदृश हैं।
ये सन्त जानते हैं कि यह सांसारिक जीवन निस्सार है। इसका केवल एक ही अर्थ है कि इसे 'साधना का क्षेत्र' रूप में स्वीकार करें। हम पशुओं के जीवन को जैसा समझते हैं वैसा ही आत्मनिष्ठ आत्माएँ सिद्धान्तहीन मनुष्य के जीवन को समझती हैं जो प्रयोजन-विहीन जीवन यापन करता है।
इस संसार में तुम कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। यदि तुम एक नीम के वृक्ष के पास जाओ, किसी शाखा से एक फल चुन लो और उसे खाओ तो तुम पाओगे कि वह कड़वा है। यह कल्पना करते हुए कि उस विशेष शाखा के चुनाव में तुमने त्रुटि कर दी है, अन्य शाखाओं को छोड़ कर शायद वह अकेली ही कड़वे फल पैदा कर रही है, आप अकस्मात् दूसरी शाखा के पास जाते हैं, उससे फल चुनते हैं और पाते हैं कि वह भी कड़वा है।
आप नीम-वृक्ष से मधुर फल कैसे पा सकते हैं? लौकिक पदार्थों से आनन्द-प्राप्ति की आशा भी ठीक इसी प्रकार की होती है। संसार से कोई सुख नहीं पाया जा सकता।
एक साधु इसे अच्छी तरह जानता है। कभी-कभी पूर्व-संस्कारों वश साधु मार्ग से तनिक विचलित हो सकता है, किन्तु वह सदा के लिए पथ-भ्रष्ट नहीं होता। साधक या जिज्ञासु में विवेक और विचार सदैव सजीव रहते हैं। इसलिए यम-प्रदत्त प्रलोभनों के प्रति नचिकेता की प्रतिक्रिया जैसी ही संसारी आनन्द (प्रलोभन) के प्रति साधु की प्रतिक्रिया होती है।
श्रेय के मार्ग पर चलने की इच्छा वाला साधु प्रार्थना, जप और भगवन्नाम-संकीर्तन आदि द्वारा प्रेय के कारण-रूप मूल को ही काटने का प्रयत्न करता है। सभी सन्तों के न्यूनाधिक विशिष्ट लक्षण वही हैं—करुणा, निःस्वार्थता, पवित्रता और सर्वोपरि है बुराई के बदले भलाई वापस करना। इसको दर्शाने के लिए सन्तों के जीवन से अनेक उदाहरण लिये जा सकते हैं।
अतएव साधु-आदर्श-दिव्यता की खोज के, सत्य की खोज के आदर्श-को प्रचारित करने के योग्य होने के लिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपको चाहिए :
(१) जहाँ तक सम्भव हो, सन्तों के जीवन पर सभी पुस्तकें लाओ और उनका अध्ययन करो।
(२) अपने निजी निवास-गृह में सत्संग आयोजित करो और अपने परिवार तथा बच्चों एवं मित्रों को सन्तों का जीवन-चरित्र सुनाओ।
(३) जो धन विलासिता सामग्री में नष्ट करते हो उसे बचाओ और उस धन से सन्तों के जीवन-चरित्र वाले पर्चे तथा विज्ञप्तियाँ छपवाओ और दूर-दूर तक वितरित करो।
इस प्रकार आपका जीवन रूपान्तरित हो जायेगा। इस तरह सन्तों का सतत चिन्तन करते हुए आप स्वयं सन्त बन जायेंगे। आप दूसरों को भी उनके जीवन रूपान्तरित करने में और सन्तत्व के विकास में सहायक होंगे। यह सर्वोत्तम और सर्वाधिक व्यावहारिक मार्ग है जिसमें आप एक साधु-जीवन के आदर्श को उन्नतिशील कर सकते हैं।
१७.ध्वंस निर्माण का अग्रगामी होता है
इस पृथ्वी पर विनाश की घटना अनिवार्यतः नवीन जन्म के अग्रगामी रूप में सृजन एवं विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पायी जाती है। इसी प्रकार आत्मा के क्षेत्र में जब साधक परिपूर्णता, आनन्द, अमर जीवन और अपरिमित शान्ति, प्रकाश एवं सुख की लोकातीत अवस्था हेतु तत्पर होता है तो वह अनेक ऐसी वस्तुओं से अपने-आपको बँधा हुआ पाता है जो उसको आध्यात्मिक कल्याण और आनन्द की वांछित स्थिति तक उन्नत नहीं होने देतीं। इस पुराने मानव-रूप-धारी जीव के अनेक तत्त्व, अवांछित निम्नस्तरीय संसारी जीवन के अनेक तत्त्व उसको नीचे खींच कर अज्ञान, तिमिर, माया और अनात्मिक प्रवृत्तियों से सतत बाँधे रखने का प्रयास करते हैं। जीवात्मा का यह निम्न रूप अनेक मानवीय कमजोरियों और कमियों के रूप में पाप-पुरुष या पशु के नाम से जाना जाता है जिसका विनाश पशु-बलि के रूप में देवी शक्ति (दुर्गा माता) की वेदी पर वांछनीय है।
यदि साधक वास्तव में और लगन से परम शान्ति एवं आनन्द को पाने का इच्छुक है तो उसको प्रारम्भिक ध्वंसात्मक प्रक्रिया के लिए दृढ़तापूर्वक तैयार रहना चाहिए। यह अपने पुराने व्यक्तित्व से उन्नत होने के लिए और आनन्द एवं शान्ति से पूर्ण आध्यात्मिक चेतना की वास्तविक तेजोमयी ऊँचाई में मुक्त विचरण करने के लिए पूर्णतया अनिवार्य है। यदि उसकी सच्ची लगन अपने निम्न अहं को नष्ट करने को तैयार कर देती है, तब वह डरावनी प्रतीत होने वाली देवी माता, जीव के कल्मष-रूप में समस्त कालिमा को विनष्ट करने वाली काली का सच्चा पूजक कहा जा सकता है। हमारे आनन्द में आने वाली बाधाओं को नष्ट करने के लिए वह अपनी खड्ग और अपने भयानक रूप का प्रयोग करती है। हमारे में जो निम्नस्तरीय, अशुद्ध और अनात्मिक है, जो निम्न एवं पशुत्व है, उस सबके लिए वह भयानक है, डरावनी तथा ध्वंसात्मक है।
एक व्यक्ति देखता है कि वह इन घोर आन्तरिक शक्तियों से अपने निजी, दुर्बल व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा न तो लड़ सकता है और न इनको पराजित ही कर सकता है। अतः मातृ-पूजा का आशय तथा आवश्यकता उपस्थित होती है। वह परम दिव्य शक्ति के उस रूप की स्तुति करता है जो उसके अपने व्यक्तिगत मामले में इस पशु-वध की प्रक्रिया करने में सक्षम हो। अतः वह माँ की ओर उन्मुख होता है और श्रद्धा से उसे सम्बोधन करता है : 'हे माता! मेरे पास विकराल रूप में आओ, अपनी डरावनी खड्ग सहित मेरे पास आओ, विनाशकारी की अपनी भयानक आकृति में मेरे पास आओ और मेरे अन्दर की अनाध्यात्मिकता, अपवित्रता और जो-कुछ पशुता एवं नीचता व अनात्मिकता है, उसे विनष्ट करने में समर्थ हो।' वह भयानकता का स्वागत करता है जिससे कि वह (माँ) उसे उसमें रहने वाली बुराइयों और अशुद्धताओं से उसके अन्दर निवास करने वाले पाप-पुरुष के पंजों से छुड़ा सके। यह शक्ति देवी के विनाशकारी रूप का स्वेच्छा से आमन्त्रण है जिससे कि वह (माँ) हमारे लिए अपने स्नेह और करुणा द्वारा, हमारे अन्दर के षड्रिपुओं (काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर), हमारे अहंकार, हमारी अशुद्धता, हमारे ममत्व और व्यक्ति के निम्नस्तरीय रूप का निर्माण करने वाली समस्त वस्तुओं को विनष्ट करने का कार्य कर सके।
इसलिए काली की पूजा कुछ क्लिष्ट है; क्योंकि हम देखते हैं कि साधक का एक अंश जब मुक्ति का आकांक्षी तथा इच्छुक हो कर अनुभव करता है कि उसे व्यक्तित्व के निम्न रूप से छुटकारा मिलना चाहिए तो माया, ममता और मोह की प्रबलता उसमें होती है और यह रूप उसके लिए कठिनाई पैदा करता है कि अपने निम्न स्तर, अपनी आसक्ति, लालसाओं और तृष्णाओं को दृढ़ संकल्प द्वारा पूर्णतया नष्ट कर सके। जब वह चाहता है कि माँ काली आयें और विनाश का कार्य करें तब भी अपने निम्न आपे में रमता रहता है। अतएव उसकी भगवती माँ काली की पूजा सम्पूर्ण हृदय से नहीं होती।
दिव्य माँ का सच्चा पुजारी वही है जो समस्त आसक्तियों को कुचलने, अपने भ्रम को कुचलने, अपनी लालसाओं को कुचलने, राग-द्वेष को कुचलने, अपने अहंकार का उन्मूलन करने को कृत-संकल्प हो और इस प्रकार मातृ-पूजा के माध्यम से जिस शक्ति का आवाहन करता है, उससे सक्रिय सहयोग करना है, अन्यथा पाखण्डी पूजा होगी।
देवी के सच्चे साधक और पुजारी को चाहिए कि अपने विचार, विवेक और वैराग्य का दृढ़ और निश्चयात्मक मन से सतत अभ्यास करे। इन समस्त उच्च गुणों का अभ्यास निम्न तत्त्वों को पूर्णतया विनष्ट करने के लिए है और यह देवी माँ की सच्ची पूजा का रूप प्रस्तुत करता है। एक साधक अपने मन और हृदय की अशुद्धताओं को ध्वंस करने तथा अपने अहंकार और निम्न स्वभाव की आसक्तियों को भस्म करने के लिए जो साधना करता है, वही पूजा माँ की असली पूजा है। किसी के द्वारा पूर्ण हृदय, गहरी श्रद्धा और अपनी समग्र सत्ता से साधना करने से ही माँ की वास्तविक पूजा गठित होती है।
प्रत्येक साधक में माँ की पूजा एक प्रक्रिया है जो तब तक लगातार चलती रहती है जब तक वह दृढ़तापूर्वक लालसाओं और आसक्तियों को, जो उसे निम्न स्थिति में बाँधे रखने का प्रयत्न करती हैं, दृढ़तापूर्वक विरोध नहीं कर देता और वह उस सीमा तक ही प्रतिदिन देवी माँ की पूजा करने में सफलता भी पाता है।
हम सबको देवी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सभी आवश्यक बल एवं प्रेरणा दें और आन्तरिक शक्ति दें कि हम अपने-आपको उनकी ओर पूर्ण हृदय से उन्मुख करें और हम स्वयं के इस पुनर्निर्माण में, पशुत्व के उन्मूलन में और दिव्य ज्योति प्रदान करने की देवी शक्ति के कार्य में सहयोग करें।
१८. भोगवादियों का आरोप
भोगवादी सदैव दृढ़ोक्ति में कहेगा कि राष्ट्र की अवनति का प्रमुखतः उत्तरदायी त्याग का सिद्धान्त है, क्योंकि वह सदैव जाति में अक्षमता तथा शोचनीय दुर्बलता लाया है जो कि हम आज सर्वत्र देखते हैं। इस गम्भीर आरोप में क्या कुछ सत्य है?
उसकी अपेक्षा आसक्ति और भोग ही पतन और दुर्बलता का वास्तविक कारण है। भौतिक पदार्थों का भोग आसक्ति पैदा करता है और मनुष्य को पूर्णतया स्वार्थी बनाता है। ऐसा मनुष्य कितना ही सक्रिय हो और कितनी ही व्यस्ततापूर्वक वह अपने-आपको संसार के कार्यों में संलग्न रखे, वह केवल स्वार्थी ही हो जाता है। सामान्य स्वार्थी व्यक्ति अपने अतिरिक्त किसी की रंचमात्र भी परवाह नहीं करता। उसका बल और उसका कार्य किसी के लाभ के लिए नहीं होता।
त्याग और अनासक्ति का आदर्श एक कारण है जिसने जाति और राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष के पौरुषत्व को अखण्डित बनाये रखा है। इतिहास का कोई युग (काल) ले लीजिए और आप पायेंगे कि जो सभी स्वार्थों से ऊपर उठ चुके थे और सभी निम्न आसक्तियों को निर्ममतापूर्वक त्याग चुके थे, उन महानतम व्यक्तियों ने ही देश का श्रेष्ठतम हित किया है और इतिहास की धारा मोड़ दी है। त्याग-भावना रहित व्यक्ति स्वार्थी बन गये। आप इस स्वार्थपरता के घातक परिणाम सर्वत्र लोभ, क्रूरता, भ्रष्टाचार, गलाकाट स्पर्धा, ईर्ष्या, शत्रुता और बृहत् पैमाने पर युद्ध के रूप में देखते हैं।
त्याग दृष्टिकोण को विस्तृत और अहंकार का उन्मूलन करता है। निःस्वार्थता की भावना के साथ कर्तव्य की उच्च विचारणा है कि भगवान् समस्त कर्मों और त्यागों के फल का, अन्ततोगत्वा, स्वभावतः उत्तराधिकारी है। त्याग के बिना व्यक्ति का दृष्टिकोण आत्मपरायणता और निजी हितों रूपी बादलों से प्रच्छन्न रहता है। दोष स्वीकार करने का उसमें साहस नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति नैतिक साहस-विहीन होता है। जब आत्म-परित्याग या आत्म-बलिदान के महान् कार्य का निर्देश आता है तो त्याग की भावना से सम्पृक्त व्यक्ति निर्भयतापूर्वक इसका पालन करता है। जहाँ व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं है, वहाँ वह अपने निजी हित की तथा अपने परिवार की भलाई पर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका से डगमगा जाता है और पीछे हट जाता है। अपने स्वार्थी पर्यावरण में ऐसी आसक्ति उसे अदृढ़ बना देती है। यदि व्याधि है तो निस्सन्देह आधारभूत व्याधि यही है।
यह महान् भ्रम के कारण है और हमारी आध्यात्मिक विरासत की विरोधी है। मानो हमारा आलस्य और अवनति का युग आ गया है। निस्सन्देह! अभागी आध्यात्मिकता के अशोभनीय गतिरोध का अधिकांश कारण है हमारे शास्त्रों का छिछला और स्वार्थपरक विश्लेषण, उस वर्ग के पण्डितों द्वारा जो हमारे देशवासियों की धार्मिक कट्टरता और भोली श्रद्धा पर पनपते हैं। लेकिन निश्चय ही इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस अवनति के लिए अपनी विरासत के प्रति पूर्ण अज्ञानता के कारण, विरोधी धाराओं के एक समूह में उचित का निश्चय करने हेतु मन्द, छिछली, धुँधली दृष्टि के कारण, अपनी अन्ध अनुकरणीय विपरीत और वृथाभिमानी दूसरों के आदर्श वाली पूजा के कारण आधुनिक तथा पश्चिमी सभ्यता में रँगा मनुष्य भी उतना ही उत्तरदायी है।
बिना त्याग की सच्ची भावना के न कोई वास्तविक सेवा, न कोई सच्चा सामाजिक कार्य, न वास्तविक परोपकार, न सच्ची देश-भक्ति और न राष्ट्रीय विकास ही हो सकता है। त्याग सर्वोत्तम शक्ति है। अतः यह हमारी जाति का केन्द्रीय (मूल) आदर्श है।
१९. गुरु और शिष्य
गुरु-कृपा एक आश्चर्यजनक रहस्यात्मक तत्त्व है जो कि साधक को जीवन के परम लक्ष्य-आत्म-साक्षात्कार या भगवद्-दर्शन अथवा मोक्ष-को खोजने और पाने का अधिकारी बना देता है। गुरु-कृपा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवर्तित होने वाले समस्त सामान्य नियमों को एक ओर रख देती है और शिष्य को, चाहे अधिकारी हो अथवा अनधिकारी, अलौकिक आनन्द तक ले जाती है।
निश्चय ही इस कथन में तथा तथ्य में किंचिन्मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है कि गुरु सदैव दयावान् होते हैं, तब गुरु-कृपा न केवल प्रदान की जाती है, न केवल दी जाती है, वरन् प्राप्त भी की जाती है। इसे प्राप्त करते समय हम अपने-आपको अमर और दिव्य बना लेते हैं।
गुरु की आज्ञा का पालन करने में प्रफुल्लता होनी ही चाहिए और इस बात की तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए कि मैं आज्ञाकारी बनूँ। शिष्य होने के नाते आपको स्वप्न में भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस आज्ञाकारिता की प्रवृत्ति को पूर्णता तक पहुँचाने के लिए हमारी साधना अहोरात्र चलनी चाहिए। यह साधना का बहिरंग है।
शिष्य के लिए गुरु का स्वरूप मानवीय नहीं होता। हमें गुरु के मानवीय पक्ष की ओर से पूर्णतया दृष्टिहीन होना चाहिए। हमें केवल देवत्व, जो कि वे हैं, का ही ज्ञान रखना चाहिए। तभी निम्न मानव से उठा कर देवत्व में रूपान्तरित कर देने वाली उनकी कृपा पाने के हम अधिकारी होंगे। हमारा गुरु से सम्बन्ध शुद्धतया दिव्य एवं शुद्धतया आध्यात्मिक है।
इस प्रकार सर्वप्रथम अपने में चेतना प्रबुद्ध करनी होगी कि हम अमर हैं और तत्त्वतः हम सच्चिदानन्द हैं। तब हम गुरु से उस सच्चिदानन्द चैतन्य की माँग कर सकते हैं और गुरु हमको वह देने में समर्थ होंगे।
आध्यात्मिक जगत् में धैर्य और विनम्रता को दशकों पर्यन्त बना रहना चाहिए। आवश्यकता हो तो श्वान की भाँति गुरु की देहरी पर आजीवन प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसमें कोई हानि नहीं है; क्योंकि अमर जीवन और मोक्ष ही हमारा लक्ष्य है।
सर्वश्रेष्ठ बात है कि नम्रतापूर्वक सब-कुछ गुरु पर छोड़ दो- 'मैं नहीं जानता कि मैं शिष्य हूँ कि नहीं। अतः हे दया और करुणा के सागर! विनती है कि मुझे उपयुक्त शिष्य बनाइए। मुझमें वह मुमुक्षुत्व उत्पन्न कीजिए, जो मुझे एक शिष्य बनाये और मुझे स्वेच्छा से आज्ञा-पालन की भावना प्रदान करे। अपने आदेशों के अनुसरण करने के प्रयत्नों में मुझे सहारा दें। आप द्वारा निर्धारित आदर्श पर अपने-आपको मोड़ने हेतु किये जाने वाले प्रयत्नों में मुझे सहारा दें।' यह हमारी सतत प्रार्थना होनी चाहिए। एकमात्र इससे हम अपने गुरु की कृपा कर्षित करने योग्य हो जायेंगे और अपना जीवन सफल बनायेंगे। प्रार्थना की परिनिष्पन्न विधि आज्ञाकारिता में और सच्चा शिष्य बनने हेतु यथाशक्य प्रयत्न करने में है।
२०. धर्म
सत्ता चूँकि एक है, समस्त प्राण-सत्ता एक है। समस्त प्राण-सत्ता मूलतः एक है; अतः मानव-जाति भी एक है। एकरूपता आध्यात्मिक क्षेत्र का नियम है। यद्यपि बाह्यतः विभिन्नता या अनेकरूपता दृश्यमान विश्व में प्राकृतिक नियम है, इसके अन्तःस्वरूप में एकरूपता या एकता जीवन का सत्य है। मानव-जाति एक है। इस प्रकार एक ओर सम्पूर्ण विश्व में हम मानव-जाति की यह एकता पाते हैं, दूसरी ओर ईश्वरत्व के सम्बन्ध में भी हम ऋषियों की उक्तियाँ पाते हैं, 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म।' ईश्वर एक है। पूर्ण एकता को एकत्व का गुण ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार इस निरीक्षण से और इस दृष्टिकोण या दृष्टि-बिन्दु से जब हम धर्म के सत्य में प्रवेश करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्म भी एक ही है। विविध धर्मों के बाह्य रूप में प्रत्यक्षतः चाहे जो भी अन्तर हो, पर उन सभी की आन्तरिक प्रक्रियाएँ अनिवार्यतः एक-समान होती हैं। मनुष्य की क्रियाओं को ईश्वरत्व की ओर धर्म ही उपलक्षित और व्याप्त करता है।
धर्म की प्रक्रिया मनुष्य को उन तत्त्वों से विमुक्त करने की है जो उसको इस दुःख और मृत्यु की भौतिक सत्ता से बाँधते हैं। यदि अनाचार ही क्लेश की उत्पत्ति का कारण है तो सदाचारी बनो। यदि असत्य के कारण मनुष्य इस सन्तापदायक नश्वर जीवन के बन्धन में आता है और उसे क्लेश और वेदना के रूप में एक भारी दण्ड चुकाना पड़ता है तो असत्य का परित्याग करो, सत्यवादी हो जाओ। यदि क्रूर होने से तुम्हें पीड़ा, सन्ताप और क्लेश की फसल काटनी पड़ेगी तो क्रूरता को उतार फेंको और अहिंसा का पालन करो, अच्छे बनो, दयावान् बनो, करुणावान् बनो। इस प्रकार जीव को इस भौतिक जीवन और इसकी वेदनाओं और दुःखों से बाँधने वाले कारणभूत तथ्यों का अध्ययन करते हुए धर्म की प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से विकसित होती है। अतः हमें अपना जीवन सतर्कता से इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए कि हम उन बातों में त्रुटि न करें जिनका परिणाम वेदनापूर्ण अनुभव और सत्ता में हो।
धर्म की प्रक्रिया शनैः-शनैः आपके लिए जीवन की योजना तैयार करती है जहाँ पर आपको अपने आत्मनिष्ठ दैवी रूप के इन सभी आदर्श जीवन-परिवर्तन-कारक तत्त्वों को प्रकट या तीव्रता से व्यक्त करना पड़ता है। इस प्रकार धर्म पाशविक रूप को दमन करने में सहायता करते हुए दिव्य स्वरूप को, जो कि पहले से ही तुम्हारी अन्तःचेतना का अनिवार्य अंग है, क्रमशः खोलता है। ईश्वर की प्रतिमा के आधार पर मनुष्य की रचना हुई है। अतएव ईश्वरत्व उसकी वास्तविक अन्तरात्मा का सार-तत्त्व है। इसलिए निम्न स्वभाव के बाह्य व्यापार को जीतना और दूर करना है। इस प्रकार दिव्य स्वरूप के प्रकटीकरण के लिए पूर्ण अवसर देना है। मनुष्य में दिव्य चेतना के प्रस्फुटित और विकसित होने के साथ ही वह तुरन्त असीम दिव्य सत्ता, सच्चिदानन्द से संयुक्त हो जाता है। एकता जो कि अज्ञानतावश कुछ समय के लिए आवरण में थी, पुनः स्थापित हो जाती है। इस धार्मिक खोज की पूर्णता पर मनुष्य घोषित करता है : 'मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि नहीं हूँ। मैं सत्-चित्-आनन्द ब्रह्म हूँ।' यह अनुभव की परिपूर्णता से और उच्च कोटि की धार्मिक साधना से आता है और यह धार्मिक साधना आपकी ईश्वर से अमर आध्यात्मिक एकता का अनुभव है।
कोई धर्म आपको भौतिकता के इस निम्न जीवन से बँधे रहने देना नहीं चाहता। सभी धर्मों का लक्ष्य पूर्णत्व की प्राप्ति, मोक्ष और अमरत्व है। सभी धर्मों की प्रक्रिया भी तत्त्वतः वही रहती है, चाहे जो भी अन्तर उनके धार्मिक संस्कारों की विधि या क्रिया-पद्धति में हो। वास्तविक धर्म निम्न स्वभाव का, मनुष्य में पाशविक अंश का पूर्ण तिरोभाव और दिव्य स्वरूप का प्रगामी प्रस्फुटन चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि के आरम्भ से ही सभी धर्मों के मुख्य सिद्धान्त और चरम लक्ष्य समान हैं।
धर्म या तो उपनिषद्, वेद जैसे शास्त्रीय पाठ्य ग्रन्थों में निहित प्रज्ञा-बुद्धि से उद्भूत हैं या परमात्मा से प्रेरित महान् ज्ञानी जनों से जो ईश्वर को प्राप्त करने की विधि के सम्बन्ध में उस (ईश्वर) का सन्देश देने के लिए प्रेरित हो कर आते हैं। यदि हम स्रोत की ओर जायें और ईसामसीह, मुहम्मद, जोरस्थ, बुद्ध के महान् और प्रेरणादायक जीवनों को देखें और संसार में विभिन्न मतों के महान् उत्स का निरीक्षण करें तो हम पायेंगे कि दृष्टान्त योग्य जीवन के माध्यम से और अपने व्यावहारिक उदाहरणों से उन्होंने हमें दिखा दिया है कि उन्होंने मानव जाति को जो धर्म दिये हैं, उनकी असली आत्मा क्या है? उन्होंने धर्मों का व्यावहारिक आचरण प्रदर्शित किया है जो कि बाद में उन्होंने अपने अनुयायियों को दिया और इन व्यक्तिगत जीवन्त प्रदर्शनों में वे सब एक-समान थे।
हम इन महान् ईश्वर-दूतों की भविष्य-सम्बन्धी उक्तियों की जाँच करें। क्या कोई ऐसा धर्म है जो हमसे कहता हो, 'असत्य बोलो, बेईमान (धूर्त) बनो, लोगों से घृणा करो, क्रोध और शत्रुता का विकास करो, अशुद्ध बनो, अनैतिक बनो ?' 'नहीं, निश्चय ही नहीं' - दृढ़ उत्तर होगा। प्रत्येक धर्म पूर्ण पवित्र, करुणामय, स्नेहमय, भक्तिमय, शीलवान्, त्यागमय जीवन और मनसा-वाचा-कर्मणा अच्छाई के जीवन पर जोर डालता है। प्रत्येक धर्म ने अपने पन्थ वालों को जीवन यापन की आदर्श पद्धति दी है। जिससे कि जीवन का लक्ष्य अर्थात् जन्म-मृत्यु, व्याधि और आपदा से रहित आत्यन्तिक अक्षुण्ण सुख प्राप्त कर सके। प्रत्येक महान् धर्म में एक-सी पद्धति या साधन हैं। यह शुद्ध और भक्तिमय जीवन भविष्य- वक्ताओं, सन्तों और मनीषियों में से प्रत्येक ने व्यवहार में प्रदर्शित किया है।
अतः धर्म तथा आध्यात्मिकता के विषय को किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें और उसका अध्ययन करें, जिस किसी भी दृष्टिकोण से आप इस पर विचार करें, आप पायेंगे कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण तथ्य मूलतः सभी मतों में वही है। सभी मत एक हैं और सभी भागवत पुरुषों ने पूर्ण नैतिक, दिव्य करुणा, अच्छाई और मानव-जाति की एकता के बोध में उसी प्रकार का जीवन यापन किया है। इस प्रकार चाहे जितना हम इन वास्तविकताओं से आँखें बन्द करने का प्रयास करें, एक प्रकार के रहन-सहन को प्रत्येक मत और धर्म की अपनी मूलभूत शक्ति के माध्यम से अनिवार्य पद्धति घोषित करते हुए हम सभी मतों में एकता पाते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी धार्मिक उपलब्धियों की प्रक्रिया में एकता है और उस चरम उद्देश्य में एकता है जो कि इन विभिन्न धर्मों में से प्रत्येक अपने मतावलम्बियों को अनुभव कराना चाहता है। ये विभिन्न मत, जैसा कि कहा गया है कि अनेक सुन्दर सुमन हैं, सुन्दर गुलदस्ता निर्मित करते हैं जिसको हम सर्वशक्तिमान् परमात्मा को अर्पित करते हैं।
२१. संन्यास की महिमा
सत्यान्वेषक होने के नाते हमें सर्वप्रथम मन में स्मरण रखना है कि संन्यास हमारे जीवन को द्विविध रूप से व्याप्त करता है। अपने विशुद्ध आध्यात्मिक रूप में संन्यास निवृत्ति की उच्चतम भावना को मूर्तिमान करता है अर्थात् नाम-रूप को पूर्णतया नकार कर नाम-रूप से परे परम सत्य अर्थात् ब्रह्म या आत्मा का अधिकारपूर्ण और सप्रयोजन आग्रह करता है। यह उच्चतम वेदान्तिक साधना का श्रेष्ठतम परिणाम है। यह भारतवर्ष की संस्कृति के अन्तर का मर्मस्थल है, हिन्दूमतानुसार मानव की सत्ता का सर्वोच्च और एकमात्र लक्ष्य है। आत्मा को आनन्दपूर्वक चेतना में सदैव लीन (मग्न) बने रहने के लिए न केवल इस भौतिक विश्व की उपेक्षा की जाती है, बल्कि अगणित विश्वों की उपेक्षा की जाती है जो कि सच्चिदानन्द के असीम सागर में एक बूँद जैसे स्थित हैं।
इस महान् साध्य और लक्ष्य के साक्षात्कार हेतु हमारे प्राचीन ऋषियों और सन्तों ने हमारे सामाजिक जीवन की रचना को चार आश्रम-रूपी ताने-बाने से मिला कर बुना है यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जिससे कि एक व्यक्ति के जीवन में सीढ़ी-दर-सीढ़ी इस आत्मा का शनैः-शनैः प्रस्फुटन हो सके। ब्रह्मचर्य-आश्रम या विद्यार्थी-जीवन में अपने समस्त उद्वेगकारी विचारों को त्यागते हुए और पूर्णतया अपने-आपको शास्त्रों के अध्ययन में लगाते हुए आत्म-नियन्त्रण, पवित्रता, सादगी, आत्म-संयम, अध्ययनशीलता, गुरु की सेवा और आज्ञाकारिता का जीवन यापन करते हुए अपने गुरु के साथ रहना पड़ता है। अगले आश्रम में वह निःस्वार्थता, आत्म-त्याग, आत्म-शून्यता के सिद्धान्तों से युक्त एक गृहस्थ का आदर्श जीवन यापन करता है। यह आगामी आश्रम अर्थात् वानप्रस्थ के लिए तैयारी है जिसमें उसे संन्यासाश्रम में प्रवेशार्थ अपने-आपको अनुशासित करना पड़ता है।
जिस व्यक्ति ने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने मित्रों के प्रति अपने समस्त कर्तव्य पूरे कर लिये हों, उसके लिए संन्यास-जीवन में ध्यान और अपने जीवन यापन हेतु भोजन प्राप्त करना ही निर्दिष्ट धर्म है। उसमें अब कोई ममता शेष नहीं रह जाती है। उसे बस केवल एक महान् कर्तव्य अर्थात् आत्मा का ध्यान और उसका साक्षात्कार करना है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के अन्तिम चरण अर्थात् संन्यास में हम सर्वश्रेष्ठ भावना रखते हैं जिससे आत्मा ससीम से उठ कर असीम में लीन होती है। जो भी आत्मा समस्त परिमित प्रतिबन्धों को तोड़ने का प्रयास करती है और समस्त आसक्तियों के संस्कारों को उतार फेंकती तथा द्वैतात्मक माया एवं दृश्यात्मक सत्ता को पूर्णतया क्षय करते हुए आत्मिक चेतना के वैभव में ऊँचे चढ़ने (विचरने) का प्रयास करती है, उन सबकी यह स्वाभाविक और शक्तिमान् गतिशीलता है।
व्यक्ति की यह आन्तरिक अभिलाषा ही संन्यास का आध्यात्मिक पक्ष है जिसके लिए कोई सामाजिक आश्रम नहीं है। यह जीवात्मा के आग्रह की गम्भीरता पर दृश्य जगत् की क्षणभंगुरता और अपने स्वरूप के चिरन्तन सत्य के प्रति उद्बुद्ध जीव के आत्म-साक्षात्कार की पिपासा पर निर्भर करता है। संन्यास का वास्तविक अर्थ और सच्ची महत्ता सन्तों और ईश्वरीय पुरुषों जो कि संन्यास के, सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ संन्यास के जीवन्त मूर्तिमान् स्वरूप हैं, के श्रद्धापूर्वक निरीक्षण से सर्वाधिक समझी जा सकती है। वे संन्यास शब्द के सच्चे अर्थ वाले व्यक्तित्व हैं। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज सच्ची संन्यास-भावना के वास्तव में महान् उदाहरण हैं। उनका प्रत्येक कार्य वास्तविक संन्यास के रहस्यों को प्रकाशित करने वाला है।
संन्यास-भावना को अज्ञानवशात् शान्ति हेतु एक प्रकार का विश्राम-स्थल एवं जीवन (संघर्ष) का सामना करने की अक्षमताजन्य पलायन समझा गया है। इस प्रकार का संन्यास तो स्वयं में निन्दनीय है। संन्यास असीम शक्ति है। भौतिक जीवन के सक्रिय संघर्ष से पलायन करके कोई व्यक्ति अपने प्रारब्ध से बच कर नहीं निकल सकता। यह एक भ्रम है जिसको कि कर्म-सिद्धान्त न जानने वाले ही मानते हैं। जो जानता है, वह जीवन के संघर्ष से बचने के लिए ज्वलन्त संन्यास-आश्रम में प्रवेश करने का साहस नहीं करेगा। नियति यह बतायेगी कि वह कैसी विकट भूल कर रहा है। जिन कर्मों से उसने सांसारिक जीवन में बचना चाहा था, वे ही उसके सम्मुख बेरहमी से निर्दयतापूर्वक खड़े हो जाते हैं और उसको उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज के सदृश कई गुने रूप में करना ही पड़ता है।
संन्यास शौर्य पर आधारित है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वास्तविक सैनिक वह है जो जीवन को यथावत् देखने का साहस करता है, जो जानता है कि संसार में प्रत्येक वस्तु स्वप्नवत् क्षणिक है और इस दृढ़ विश्वास को मानने का साहस करते हुए कि संसार मिथ्या है, वह ऐन्द्रिक विषयों की आसक्ति के दृढ़ बन्धनों से ऊपर उठ गया है और ऐसे जीवन में प्रवेश कर गया है जहाँ सभी संघर्षों में से भीषणतम संघर्ष, अपनी स्वयं की प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष से उसे निपटना होता है। 'मैं रूपवान् हूँ, प्रतिभावान् हूँ' की भावना तथा सामान्य मानव-चेतना में संवेष्टित सभी संस्कार-समुदायों तथा अध्यासों को उन्मूलन करने और उनके स्थान में 'मैं यह शरीर नहीं हूँ', 'मैं यह मन नहीं हूँ', 'मैं सच्चिदानन्द आत्मा हूँ', 'मैं सर्वव्यापी, असीम, जन्म-मृत्यु से परे तथा अनन्त शक्ति-सम्पन्न हूँ', इस महान् चेतना को शनैः-शनैः प्रवेश कराने से अपेक्षातर अधिक कठिन प्रयास संसार में कोई नहीं है। यही वास्तविक वीरता है। ऐसा करने के प्रयत्न में व्यक्ति को युगो पुराने उन विचारों से युद्ध करना पड़ता है जिन्हें उसने जिन करोड़ों योनियों के मध्य से जीव-सम्बन्धी चेतना गुजरती चली आयी है, उनके माध्यम से प्राप्त किया है। यह एक दिन का संघर्ष नहीं है। यह जीवन-भर चलने वाले संघर्ष का रूप ले सकता है और बहुत बार व्यक्ति को पराजय एवं पतन का सामना करना पड़ता है।
संन्यासी कभी कायर (कापुरुष) नहीं होता। उसकी वीरता इस तथ्य में ही निहित है। वह असफलता या प्रत्यावर्तन को स्वीकार नहीं करता। उसके लिए संघर्ष के ये सभी तत्त्व उस महान् आदर्श के, उस महान् लक्ष्य के निकट और निकटतर पहुँचाने वाली सीढ़ियाँ हैं जिस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने पर वह घोषित करने में समर्थ होगा : "देहो नाहं, जीवो नाहं, प्रत्यगभिन्नो आत्मैवाहम् "मैं यह शरीर नहीं हूँ, न जीव हूँ, मैं अन्तर्तम अविभक्त आत्मा हूँ। प्रत्येक कृत कर्तव्य प्राप्तव्य के रूप में ही है, हानि के रूप में कभी नहीं होता।
संन्यासी वह है जिसका जीवन उत्कृष्ट त्याग एवं पूर्ण निष्कामता पर आधारित है। उसको इस स्थूल भौतिक बाह्य विश्व के समस्त सुखों की इच्छाओं को तथा स्वर्ग के परमानन्द के भोग की कामना को भी त्याग देना पड़ता है। एक संन्यासी के लिए घास की पत्ती से ले कर उच्चतम ब्रह्म तक सभी मिट्टी के समान हैं। वह इनसे ऊपर उठ जाता है और अपने आत्मिक स्वरूप को दृढ़तापूर्वक घोषित करता है। इसलिए उसका जीवन त्याग पर अवलम्बित होता है। चाहे उसके स्थूल शरीर की प्रशंसा हो या निन्दा, मान हो या अपमान, वह उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देता। वह आत्म-चेतना में निवास करने को सदैव प्रयत्नशील रहता है। उपर्युक्त वार्ता को मनन कर निर्णय करें कि आप क्या हैं?
एक संन्यासी का जीवन तीन तत्त्वों से निर्मित है-पूर्ण त्याग, असीम के लिए ज्वलन्त अभीप्सा तथा निर्मल पवित्रता। पूर्ण त्याग उसके जीवन का नकारात्मक पक्ष है। ज्वलन्त अभीप्सा उसके जीवन के मध्य में सकारात्मक पक्ष है। निर्मल पवित्रता वह तन्तु है जिससे उसका जीवन बना है। सकारात्मक पवित्रता, उसकी पात्रता में दिव्य चेतना के अवतरण की एक शर्त है। संन्यासी के जीवन का यह एक आदर्श नमूना मानते हुए अपनी अहंकारमयी चेतना के मध्य से काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर के ज्वर से तथा केवल संन्यास के सही ज्ञान तथा ब्रह्म-चिन्तन से ही दूर हो सकने वाली इस सांसारिक व्याधि से बाहर निकल पाने के लिए आयें, हम सभी मिल कर संघर्ष करें। यदि समस्त वेदनाओं और दुःखों का सदा के लिए निवारण करना है तो हमें संन्यास ग्रहण करना चाहिए। यदि हमारा अग्रिम जीवन शान्ति और आनन्द के रूप में देदीप्यमान होना है तो संन्यास और एकमात्र संन्यास ही पथ है; क्योंकि इस पृथ्वी पर स्वार्थपरता ही समस्त आपदाओं के, सम्पूर्ण झगड़ों एवं विवादों के, सभी समस्याओं के, सभी युद्धों और शत्रुताओं के मूल में है। आज के मानव-समाज में परिव्याप्त प्रत्येक दुःख और प्रत्येक आपदा के मूल में आसुरिक लक्षणों वाली स्थूल स्वार्थपरता ही है जहाँ मनुष्य प्रत्येक वस्तु अपने लिए चाहता है और यह चिन्ता नहीं करता कि अपने लिए वस्तुएँ पाने की लालसा की पूर्ति की प्रतिक्रिया में दूसरों पर क्या बन आती है? संन्यास इस आसुरिक लक्षण को मूल में ही काट देता है; क्योंकि संन्यास निःस्वार्थता और स्वार्थपरता के त्याग पर आधारित है और यदि स्वार्थपरता का त्याग कर दिया तो सभी वस्तुओं का त्याग हो गया । मैं तो ऐसा कहूँगा कि स्वार्थपरता के त्याग का अर्थ है सभी इच्छाओं का त्याग; क्योंकि स्वार्थपरता ही व्यक्ति में अनेक इच्छाओं का रूप धारण करती है। इसलिए संन्यास की सही भावना को सरल शब्दों में वर्णन किया जा सकता है-पूर्ण निष्कामता। इसके प्रकाश में अपने जीवन पर विचार कर उसका मूल्यांकन करें और निश्चय करें कि आप कहाँ पर स्थित हैं। नये रूप से संकल्प लो और आगे बढ़ने की ओर साहसपूर्वक प्रयत्न करो।
प्रत्येक उत्साही साधक और सच्चे संन्यासी का यह कर्तव्य है कि वह दो महत्त्वशाली तत्त्वों को -अधिकारी (मान्य) शास्त्रों में वर्णित संन्यास की धारणा तथा इस महान् देश की प्राणभूत परम्परा द्वारा अमरत्व प्रदान किया हुआ व्यक्ति जीवन में संन्यास का व्यावहारिक आचरण-हृदयांकित करने का अवश्यमेव प्रयत्न करे। सच्चा विवेकशील हिन्दू संन्यास का क्या आशय लेता है? हम जानते हैं कि संन्यास जीवन का चतुर्थ आश्रम है। व्यक्ति जीवन के इस आश्रम में प्रवेश करते समय गुरु द्वारा दीक्षा पाता है और विरज होम सम्पन्न करता है। संन्यास के आशय के सम्बन्ध में यह विरज होम ही सही सूत्र (मार्गदर्शक सिद्धान्त) और सही उत्तर तुम्हें देता है। विरज होम संन्यास के सच्चे अर्थ पर पुंजीभूत प्रकाश डालता है। संन्यास का अर्थ है पुरानी मायावी, अहंकारी चेतना को शून्य कर देना। इसका अर्थ है समस्त इच्छाओं और आसक्तियों को पूर्ण त्याग की ज्वलन्त अग्नि में भस्मसात् करना। इसका अर्थ है शारीरिक चेतना का अन्तिम अवशेष राखवत् बना देना। यह एक दिव्य नवीन चेतना का उद्भव होगा। 'मैं न तो शरीर हूँ, न मन, अमर आत्मा हूँ मैं'- ऐसी चेतना होती है एक संन्यासी की जिसका तन, मन, इन्द्रियाँ, प्राण और अहं सभी की विरज होम की लपटों में आहुति दे दी गयी है। यह सर्वश्रेष्ठ त्याग है। इसलिए संन्यास का आशय है सर्व त्याग। अतः उसका दैनिक संकल्प होता है : 'मैं भूलोक के सुख का त्याग करता हूँ। मैं भुवर्लोक के सुख का परित्याग करता हूँ। मैं स्वर्गलोक के सुख का त्याग करता हूँ।'
इस लोक की या परलोक की किसी भी वस्तु के प्रति कामनाएँ शून्य हो जाती हैं। इस सन्धि पर हम आश्चर्यजनक दैवी प्रकाशन पाते हैं। इस महान् त्याग के शिखर पर एक अन्य संकल्प आता है और संन्यासी घोषणा करता है, 'मैं किसी जीव के लिए भय का कारण नहीं बनूँगा।' संन्यासी सभी जीवों को पूर्ण निर्भयता का वचन देता है, जिससे किसी जीवधारी को उससे कोई हानि होने के भय की आवश्यकता नहीं है। इससे वह अपने-आपको विश्व-प्रेम या विश्व-बन्धुत्व का संकल्प लेता है; क्योंकि भय केवल वहीं होगा जहाँ हानि या पीड़ा की सम्भावना हो और उत्तरोक्त केवल वहीं विद्यमान होंगे जहाँ घृणा या शत्रुता वर्तमान हो। लेकिन जहाँ प्रेम ओत-प्रोत हो, वहाँ केवल स्नेहमयी सेवा और आनन्द बहता है और सभी जीव निर्भयतापूर्वक इसमें पूर्ण आश्वासन और विश्वास के साथ सहभागी हो सकते हैं। इसलिए ऐसा विश्व-प्रेम और सेवा महात्याग की सहज उपशाखा होगी। अतः ये दो बृहत् और विशिष्ट त्याग के तत्त्व अर्थात् नाम, यश, पारितोषिक की कामनाओं का त्याग तथा सेवा अर्थात् बीमार, दरिद्र और अभावग्रस्तों की सेवा-संन्यास की भावना को निर्मित करने के तत्त्व हैं। त्याग आत्म-साक्षात्कार या आत्मज्ञान के लिए है। अतः सेवा और आत्म-साक्षात्कार आदर्श युगल प्रवृत्तियाँ बनाते हैं जो परम सत्य की सर्वोच्च चेतना को प्राप्त कराने की ओर ले जाते हुए सच्चे संन्यासी के जीवन में क्रियाशील रहती हैं।
२२. मानव-मन का विश्लेषण
मनुष्य को एक विचारशील प्राणी की संज्ञा दी गयी है। उसका वह भाग, जो तर्क-शक्ति से युक्त है, उसके मानव-स्वभाव को निर्मित करता है और यह उसके व्यक्तित्व का केन्द्र है। एक ओर चेतना की उच्चतर स्थिति की आकांक्षायुक्त उसका सारभूत, नित्य शुद्ध तथा पूर्ण दैवी स्वभाव है जो कि अजन्मा, अक्षय, अविनाशी और अमरत्व की सत्ता के स्वभाव का है, उसका वास्तविक स्वरूप है और जो स्थूल शरीरोपरान्त भी, यहाँ तक कि मन के क्रिया-कलाप बन्द हो जाने के पश्चात् भी निरन्तर रहता है। भौतिक शरीरोपरान्त जब एक जीवन-काल समाप्ति पर आता है, व्यक्ति के समस्त मानसिक व्यापार समाप्त हो जाते हैं और समस्त ऐन्द्रिक व्यापार भी, जो विचार-प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, समाप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। हम देखते हैं कि किसी के मानसिक व्यापार बन्द हो जाने के पश्चात् भी, मानव का सरूप अर्थात् चेतना निरन्तर बनी रहती है। अन्तर्प्रज्ञा-सम्पन्न ऋषियों ने आध्यात्मिक शोधों से ऐसी खोज की है कि यह चेतना की इकाई श्रृंखलावत् कड़ी-दर-कड़ी निरन्तर यात्रा करती है और मानव-शरीर-धारी उस श्रृंखला की एक कड़ी है, अतः शरीर-विसर्जन के और मानसिक व्यापार के स्तब्ध हो जाने के पश्चात् चेतना की निरन्तरता के सम्बन्ध में जो बहुत बड़ा सन्देह रहता है, उसका निराकरण दो प्रकार से हुआ है : पूर्व-जन्म की स्मृति किसी व्यक्ति में क्रियाशील थी। उसने अपने पूर्व-जन्म के सम्बन्ध में जो तथ्य या विवरण दिये, उनकी जाँच की गयी। वे पूर्णतः सही सिद्ध हुए। पश्चिम में चेतना की निरन्तरता कतिपय शोधकर्ताओं द्वारा कुछ निम्न स्तर पर शोध करके सिद्ध कर दी गयी है। वे विशिष्ट व्यक्तियों से उनके भौतिक शरीरोपरान्त सम्पर्क करने की क्षमता रखते थे और चेतना की निरन्तरता पर शोध करने वाले प्रमुखतम व्यक्तियों में से सर ओलीवर लाज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। वे पश्चिमी साहित्य और पश्चिमी विचारकों के मध्य बहुत विख्यात व्यक्ति थे। अब मनुष्य के इस सारभूत भाग को वह तत्त्व कहा गया है जो उसको उच्चतर महान् आकांक्षाओं की ओर सदैव आवाहन करता है। उच्चतर चेतना की प्राप्ति के लिए, जहाँ वह ऐसे अनुभव पर स्थापित हो कि दुःख उसको स्पर्श न कर सके, जहाँ अन्नमय कोश और मनोमय कोश की वेदनाएँ शान्त हो जाती हों और निरन्तर आनन्द की स्थिति उस अनुभव का चित्रण करती हो, प्रयत्नशील होता है। साथ ही हमने देखा कि केन्द्रीय मानव के, बौद्धिक स्वभाव के द्वितीय और उसके अपने स्थूल रूप में निम्न चालनाओं से निर्मित जंगली, पाशविक रूप है। निम्न ऐन्द्रिक वासनाएँ तथा अशुद्ध तृष्णाएँ प्रत्येक मानव के इस भाग का गठन करती हैं।
विश्व-प्रक्रिया सत्ता के निम्न स्तर से उच्चतर स्तर पर की क्रमिक उन्नति है और भारतीय दर्शन मानता है कि जैसे जीव-चेतना निम्न सत्ताधारी निम्न जीवनों के मध्य से गुजरती है, प्रत्येक जीवन का संस्कार, जिसके मध्य से यह गुजरती है, चेतना की गहराइयों में छूट जाता है और यह उसके पाशविक स्वभाव अथवा उसके अपवित्र स्थूल तत्त्व को बनाता है और इस प्रकार प्रत्येक जीवन-स्तर उसके अन्तस्तल में कुछ स्थूल संस्कार छोड़ जाता है। पाशविक अवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि तृष्णा के रूप में जो मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान रहती है, उस पर जीव का नियन्त्रण नहीं रहता। वे बौद्धिक विचारों से निर्देशित नहीं होते, इसलिए ये तत्त्व जीव के निम्न रूप का निर्माण करते हैं। चेतना द्वारा पशुत्व वशीभूत और अधीन किया हुआ हो, फिर भी उस दिव्यता को जाग्रत करना है जो अभी तक प्रच्छन्न है, प्रकटित नहीं है। इन दोनों के मध्य मानव-स्वभाव है जो सदा क्रियाशील, गतिशील रह कर व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार से अपने-आपको व्यक्त कर रहा है, लेकिन दैवी एवं आसुरी स्वभावों से अभिभूत है।
प्रत्येक जीव दमित किन्तु सक्रिय आसुरी स्वभाव की ओर आकर्षित रहता है। आसुरी स्वभाव प्रत्येक मानव में विभिन्न स्तरों में सक्रिय होता है, जब कि दैवी स्वभाव अभी सक्रिय नहीं हुआ; क्योंकि वह अब भी सुप्त है, अभी भी जाग्रत नहीं है। इस प्रकार व्यक्ति आसुरी स्वभाव की ओर अधिक कर्षित है। अतः यह पाया गया कि मानव-जीवन व्यक्ति के आसुरी स्वभाव और विवेक-शक्ति के मध्य का संघर्ष है जो कहता है, 'मैं सोचता हूँ, यह मेरे योग्य नहीं है, एक मानव होने के नाते मुझे यह नहीं करना चाहिए।' ये विचारणाएँ मानवीय तर्क द्वारा क्रियाशील रखी जाती हैं। कैसे ? प्रारम्भिक शिक्षण के बल पर। शैशवावस्था में वह कुछ कार्यों से बचने और कुछ कार्यों को करने में लज्जा लगने हेतु बड़ों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण और पारिवारिक विरासत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि वह एक शिक्षित सुसंस्कृत परिवार में जन्मा है तो स्वभावतः उसकी भावनाएँ अधिक परिष्कृत होंगी। जो एक असभ्य परिवार में जन्मे बहुत पिछड़े एवं अशिक्षित वर्ग के हैं, उन लोगों में तर्क कम नियन्त्रण डालेगा। यद्यपि वे भी तर्क से युक्त हैं, तथापि उनमें तर्क उतनी मात्रा में क्रियाशील नहीं जितना कि उस मनुष्य में जो कि सभ्य, सुसंस्कृत परिवार में जन्मा है। प्रारम्भिक प्रशिक्षण, वंशानुक्रमण और तत्पश्चात् उसके पूर्व-संस्कार सक्रिय होने प्रारम्भ हो जाते हैं। संस्कार का अर्थ है पिछले जन्म के पड़े हुए अनुभवों का प्रभाव।
जीवन प्रगतिशील है और प्रत्येक जन्म में मनुष्य वस्तुओं को सीखता और अनुभवों से शिक्षण ग्रहण करता चला जाता है। ये सभी शिक्षाएँ मानव-मात्र में सूक्ष्म संस्कार के रूप में रहती हैं। पूर्व-जन्म के अनुभवों और कर्मों से बने ये संस्कार ऋण या सम्पत्ति के रूप में हो सकते हैं और ये संस्कार अहंकार से मिल कर कार्य प्रारम्भ कर देते हैं जो मानव में कुछ आयु के बाद कार्यरत हो जाता है। शैशवावस्था में व्यक्तित्व क्रियाशील नहीं होता। सामान्यतः कुछ आयु के पश्चात् ही शिशु अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करने लगते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो पूर्व-जन्म के उनके संस्कार कार्य करने लगते हैं और वे प्रत्यक्षतः मनुष्य के तर्क में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर देते हैं, उसको प्रेरित करते हैं कि अमुक क्रियाओं की उपेक्षा करो। तब हम सभ्य समाज का नियन्त्रण पाते हैं। लोग कहते हैं, 'यह मत करो।'
कुछ कार्य अस्वीकृत किये जाते हैं और घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। ये प्रभाव मनुष्य के तार्किक भाग की रचना करते हैं और यह इन तत्त्वों और निम्न चालनाओं के मध्य के संघर्ष ही हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में द्वन्द्व पैदा करते हैं। आत्म-सम्मान, सुशीलता के तत्त्व-ये सब तत्त्व एक मनुष्य में कार्य प्रारम्भ कर देते हैं और वे स्थूल और आसुरी स्वभाव की चालनाओं के विरुद्ध एक सीमा तक नियन्त्रण का कार्य करते हैं।
कल्पना करो कि वह विद्वानों के सम्पर्क में आता है और ज्ञान के शब्द श्रवण करता है। उत्थानमूलक साहित्य के सम्पर्क में आता है और अधिकाधिक दिव्य बातों का श्रवण करता है। उसकी बुद्धि का संस्कार होना प्रारम्भ हो जाता है। तब निम्न अहं के ऊपर नियन्त्रण-शक्ति बलवती हो जाती है और उसको अधिकाधिक मानव-स्वभाव पर स्थापित कर देती है। वह आत्म-नियन्त्रित, आत्मानुशासित मनुष्य हो जाता है, ऐसा मनुष्य जो अपनी निम्न वासनाओं और चालनाओं के ऊपर आधिपत्य रखता हो। समाज में भय का तत्त्व भी किसी अंश तक मन की निम्न वासनाओं के नियन्त्रण हेतु कार्य करता है। कल्पना करें कि एक पुरुष गलत कार्य करता है। तो उसे दण्ड दिया जायेगा। अतः दण्ड का भय वहाँ है। विकास के उच्चा स्तरों में भय संसार से नहीं होता, लेकिन ईश्वरीय दण्ड से रहता है। ये सभी बातें उसको मानवीय स्तर पर दृढ़तापूर्वक स्थापित कर देती हैं और मानव-सत्ता के निम्न, स्थूल, अशुद्ध, आसुरी भाग की चालनाओं के अत्यधिक बार-बार के प्रकटीकरण पर प्रतिरोध के रूप में कार्य करती हैं। निःसन्देह! तब वहाँ यदा-कदा द्वन्द्व होते हैं। प्रत्येक मानव-प्राणी के जीवन में अकस्मात् कुछ क्षण आते हैं जब वह (स्त्री या पुरुष) अपने जीवन पर विचार-मन्थन प्रारम्भ करता है, 'क्या मैं किसी प्रयोजनार्थ जीवित हूँ? इन सबका क्या आशय है? अन्ततोगत्वा एक दिन मुझे इस दृश्य-पटल से एक क्षण की सूचना पर चला जाना होगा।' तब वह (स्त्री या पुरुष) अपनी जीवन-पद्धति से, जो कि वह व्यतीत कर रहा है, असन्तोष अनुभव करता है। तब किसी उच्च स्रोत से आवाहन आता है और अच्छाई के लिए, ऊपर उत्थान के लिए, जो मात्र संसारी न हो, जो भौतिक शरीर का न हो, उसको अनुभव करने के लिए एक आकांक्षा उठती है। उन समयों में मनुष्य एक दार्शनिक (विचारशील) हो जाता है और अपने इन्द्रियपरायण जीवन से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। लेकिन पुनः अपने दैनिक क्रिया-कलापों के भँवर में पड़ अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। पुनः उसके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह प्रश्न करता है, 'क्या जीवन में कोई उच्च उद्देश्य है?' यह उस जीव में उच्चतर स्वभाव की उपस्थिति का द्योतक है जो कि अनुभव एवं साक्षात्कार किये जाने की क्षमता वाला है और इस उत्थानमूलक धारा का लाभ उठाने एवं भौतिक जगत् की सामान्य नीरस क्रियाओं से उत्थान करने में सक्षम बनाने के लिए ही सभी ईश्वरीय दूत मनुष्य से निरन्तर आग्रह करते हुए कहते चले आ रहे हैं, 'तुम यहाँ क्या कर रहे हो ? तुम कब तक निद्राग्रस्त रहोगे?' वे पुनः-पुनः मानव मात्र में प्रसुप्त सारभूत दैवी स्वभाव को जाग्रत करने का प्रयत्न करते हैं। अतः मनुष्य के त्रिगुणात्मक स्वभाव का विश्लेषण करते हुए हमने पाया कि योग की प्रक्रिया का मौलिक कार्य जो सम्पन्न करना है, वह है मनुष्य के निम्न पाशविक स्वभाव को हटाना या मिटाना और मानव-चेतना को उच्च दैवी चेतना में समुन्नत करना, जहाँ वह शरीर और मन से परे हो जाता है और स्थायी आत्मानन्द के यशस्वी अनुभव एवं सत्य में, अपने मूल स्वभाव में जो उसकी चेतना के अन्तर्तम प्रकोष्ठ में प्रकाशित होता है, स्थापित हो जाता है और मनुष्य के भीतर क्रियाशील योग की गति के विश्लेषण पर विचार करते हुए हमने यह भी इंगित किया था कि यदि यही प्रक्रिया है तो सभी योग, चाहे कितनी ही अधिक उनकी बाह्य पद्धतियों में भिन्नता हो, अनिवार्यतः अपने में एक-सी प्रक्रिया कार्यान्वित करेंगे। आज हम यह विचार करने का प्रयत्न करेंगे कि विभिन्न योग वास्तव में कैसे एक ही केन्द्रीय प्रक्रिया कार्यान्वित करते हैं और किस प्रकार वे यह प्रक्रिया आरम्भ करते हैं। यह इस प्रकार है :
हम देखते हैं कि मनुष्य अपने-आपको अपनी वाणी और कर्मों से व्यक्त करता है। एक मनुष्य अच्छा है या बुरा, उसका जीवन अच्छा है या बुरा, यह केवल उसकी वाणी और कार्यों से जाना जा सकता है। यदि एक मनुष्य अति-आसुरी, अति-अपवित्र है तो वह घोर क्रूर कर्म करता है। उसके सभी कर्म अपवित्र, पापपूर्ण और हानिकारक होते हैं। वह दूसरों पर पीड़ा, अवसाद (विषाद) और विनाश लाता है। अपने सम्भाषण (बोलचाल) में वह कठोर होता है, लोगों पर लांछन लगाता है, लोगों को अपमानित करता है, लोगों को पीड़ित करता है। इस प्रकार कर्कश, क्रूर और गलत शब्दों एवं कार्यों से मनुष्य का आसुरी स्वभाव स्वयमेव इस मानव-लोक में अभिव्यक्त होता है। समस्त अभिव्यक्ति वाणी और कर्म के माध्यम से होती है। लेकिन प्राचीन काल के योगी और आत्मदर्शी सिद्ध पुरुषों ने मनुष्य की वाणी और कर्मों से परे जाने की चेष्टा की है। उन्होंने कहा, 'यह वाणी और कर्म कुछ गहरे आन्तरिक रूप में विद्यमान हैं और सर्वप्रथम जानना चाहिए कि वे कहाँ से प्रस्फुटित हुए हैं।' और उनसे कर्म एवं वाणी के मूल का पता लगाने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने अनुभव किया कि कर्म और वाणी का मूल आधार विचार है। जो मनुष्य ने विचार किया और मन में अनुभव किया कि यह केवल वही है जो बाद में वाणी और कर्म के रूप में व्यक्त किया गया।
वाणी और कर्म यद्यपि बाह्य विश्व में अत्यधिक महत्त्व वाले थे और इन्होंने मानव-जीवन के बाह्य क्षेत्र पर या तो विध्वंस किया या आश्चर्यजनक अच्छाई की। वे और कुछ नहीं, केवल अन्तःशक्ति के बाह्य लक्षण थे तथा वह शक्ति विचार-शक्ति थी। उन्होंने विचारों के अध्ययन तथा शोध-कार्य करने में अपना ध्यान तथा अपनी समस्त बुद्धिमत्ता लगायी और पाया कि उन्हें अपने मन के अत्यधिक रहस्यात्मक जटिल तत्त्व-व्यूह का सामना करना पड़ा है। वे सब उनके मानस में उठे थे। अतः मनुष्य के मन का अध्ययन, योग का सर्वाधिक महत्त्व का कार्य था। मनुष्य के मन का विश्लेषण, मनुष्य-सत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्मतम खोज, कैसे मन कार्य करता है, इसकी विभिन्न चित्तवृत्तियाँ क्या हैं, इसके अनिवार्य घटक क्या हैं आदि-ये सब योगियों के लिए विषय-वस्तु को निर्मित करते थे। उन्होंने पाया कि मन विभिन्न कार्यों से विचार करता है और इसका अभिव्यक्तिकरण भी विभिन्न तत्त्वों पर निर्भर करता है। अब वाणी और कर्म का उद्गम खोज लिया गया है—वह उद्गम विचार है और उस विचार का उत्पत्ति-स्थल भी खोज लिया गया है। ऐसा क्यों है कि कुछ प्रकार के विचार एक मस्तिष्क में आते हैं और अन्य प्रकार के विचार नहीं। वह क्या वस्तु है जो विचार को आश्रय (सम्पोषण) देती है। उन्होंने अधिक और अधिक गहरी शोध प्रारम्भ की और वे कुछ अद्भुत आविष्कार तक पहुँचे। वे आविष्कार क्या थे? उन्होंने पाया कि विचार सर्वथा विश्रृंखलित नहीं होते। मैं आपके समक्ष कुछ बहुत अधिक सरल उदाहरण प्रस्तुत करूँगा जो आपके सामने कुछ नियमों को प्रकट करेंगे जो प्रत्येक मन (मस्तिष्क) के दायरे में क्रियाशील होते हैं। ये नियम क्या है?
उदाहरणार्थ, यदि आप एक चिकित्सक को देखते हैं तो तुरन्त औषधालय का विचार, अस्पताल का विचार, औषधियों का विचार आ जाता है। यदि आप एक सैनिक को सैनिक वेशभूषा में देखते हैं तो युद्ध-सम्बन्धी विचार, टैंक और बन्दूकों के विचार, सैनिकों के बारूद भरने के विचार-ये सभी बातें मस्तिष्क में आ जाती हैं। यदि आप एक वकील को देखते हैं तो न्यायालय, वाद-बन्ध, मुवक्किल, दण्डविधानसंहिता, न्यायाधीश, दण्ड और कारागार के विचार आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में दो बातें समाविष्ट हैं-एक है हमें एक नियम का पता चला कि जैसे मानव-मन ने पंचेन्द्रियों में से किसी एक माध्यम से किसी विषय को ग्रहण किया तो जैसा पदार्थ ग्रहण किया है उसी प्रकार के पदार्थों की वैचारिक श्रृंखला वह तुरन्त प्रस्तुत करता है और तब एक-सी विचार-तरंग मन में अन्य सम्बन्धित विचारों के साथ उठती रहती है। यह संसर्ग का नियम कहलाता है। अतः इस नियम में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि कोई पदार्थ आपके नेत्रों के सम्मुख विचार प्रस्तुतीकरण हेतु रहना ही चाहिए। केवल स्मृति से आप किसी वस्तु पर विचार करते हैं तो तुरन्त स्मृति के माध्यम से मनःप्रसूत पदार्थ से सम्बन्धित विचारों की एक श्रृंखला गतिशील हो जाती है और उन्हें पता लगा कि संसर्ग का नियम वहाँ मन के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे मन के विचारों को निर्देशित कर रहा है। एक अन्य अतीव मनोरंजक नियम भी खोजा गया। उन्होंने पाया कि मन की विचित्र आदत है, मैं इसे बहुत खतरनाक, अपवित्र यानी मलिन आदत कह सकता हूँ। यह सभी साधकों के लिए सिरदर्द है। जो कुछ भी इन्द्रिय-सम्पर्क मनुष्य करता है, वह तड़ित् गति से उसका लेखा अंकित कर लेता है। गमन करते हुए आप कुछ शब्द बोलें, कुछ लोगों को देखें, आप किसी अनुभव को प्राप्त करें, तुरन्त यह विद्युत्वत् लेखा एक संस्कार के रूप में अंकित हो जाता है और योगी के लिए यह अति-महत्त्व का क्यों है? यह ऐसे संस्कार के अति-विचित्र स्वभाव के ही कारण है। संस्कार केवल चित्र-फलक पर खींची हुई निर्जीव रेखा मात्र नहीं है, बल्कि यह एक सजीव लेखा है और मैं आपको स्पष्ट करूँगा कि एक सजीव लेखा क्या है। वहाँ एक आलोक-चित्रित लेखा होता है। यदि कोई वस्तु भावात्मक प्लेट के संसर्ग में आती है तो तुरन्त यह उसका प्रतिबिम्ब ले लेती है और सदा के लिए अंकित कर लेती है, किन्तु यह केवल निर्जीव छाप है। जो चित्र फोटोग्रैफिक प्लेट ने स्वयं पर लिया है वह न आपके पास आ सकता है, न आपसे बात कर सकता है। किन्तु यह संस्कार मन द्वारा ग्रहीत एक छाप है जो अपने-आपमें एक बार फिर व्यक्ति में वह सम्पूर्ण अनुभव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जो संस्कारोत्पत्ति का कारण था। यह संस्कार के स्वभाव का अधिक महत्त्वशाली रूप है जो मानव-मन में किसी दैववशात् सम्पर्क, क्रिया-कलाप या अनुभव के द्वारा, जिसके मध्य से व्यक्ति गुजरता है, प्रविष्ट हो जाता है। प्रत्येक संस्कार अपने में स्वभावतः एक बार पुनः उसी अनुभव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसने कि मूलतः इसे उत्पन्न किया था। यदि मैं आपको आप लोगों के बाह्य जीवन-सम्बन्धी एक उदाहरण बताऊँ तो आप पूर्णतया इसे समझ जायेंगे कि यह क्या है? बृहद् वृक्ष से उससे ही पैदा हुआ एक लघु बीज पाते हैं। वृक्ष विशाल है, किन्तु बीज अति-लघु है। लेकिन तो भी इस बीज की महान् क्षमता क्या है? यद्यपि यह इतना लघु दिखता है, यह अपने-आपमें एक बार फिर विस्तार से सर्वांग वृक्ष उत्पन्न करने की प्रकृतिदत्त योग्यता या शक्ति रखता है जो कि मूलतः इसका जन्मदाता है। गतिशीलता में पोषित होने के लिए उचित पर्यावरण और अनुकूल साधन दिये जाने पर यह लघु बीज एक बार पुनः उस सर्वांग पूर्ण वृक्ष को उत्पन्न कर सकता है जो उसकी उत्पत्ति का हेतु था। यही बात संस्कार के साथ है।
कल्पना करें कि किसी ने आपको कुछ चखने को दिया। वास्तविक स्वाद केवल दो इंच या तीन इंच के जिह्वा-क्षेत्र-भर में है। वस्तु के आपकी जिह्वा के सम्पर्क में आने के पूर्व वहाँ कोई स्वाद नहीं है; एक बार गले के नीचे चले जाने पर भी वहाँ कोई स्वाद नहीं रहेगा। आप स्वाद का अनुभव तभी तक कर सकते हैं जब तक कि वस्तु आपकी जिह्वा पर है। लेकिन फिर भी वह साधारण अनुभूति त्वरित ग्रहण हो जाती है और मन में संस्कार के रूप में प्रस्थित हो जाती है। कल्पना करें कि आप उस विशिष्ट नगर या कसबे के बीच से दैववशात् गुजरते हैं जहाँ दस वर्ष पूर्व आपने किसी वस्तु का रसास्वादन किया था। जब आप उस नगर या कसबे से पुनः गुजरते हैं, पूर्व-स्मृति आ जाती है, '१९४५ में मैंने यह वस्तु खायी थी और मैंने अमुक मुहल्ले में खायी थी।' कल्पना करें कि आप कहीं बैठे हैं। एक बार आप उसके सम्बन्ध में सोचते हैं, आपको लगता है कि वह कितनी अच्छी थी। वह आपके मुँह में कैसे घुल गयी थी और इस प्रकार ऐन्द्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और यह कल्पना तुरन्त संस्कारों को काम (इच्छा) का रूप प्रदान कर देती है। प्रथमतः संस्कार वासना के रूप में रहता है और वासना वृत्ति के रूप में प्रस्फुटित होती है और मानसिक तौर से सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह पुनरोत्पादन की प्रक्रिया कल्पना की शक्ति से काम (इच्छा) के रूप में घनीभूत हो जाती है तथा एक बार कामना प्रस्फुटित होने पर प्राणी उसे पूर्ण करने का तुरन्त प्रयास करता है। वह उस कामना का दास हो जाता है। यदि एक कामना उदय हुई तो सामान्य मानव का उसकी तृप्ति हेतु प्रयत्नशील होना स्वाभाविक है। तुरन्त अहंभाव यह कहता है, 'मुझको यह प्राप्त करना चाहिए' और वह अपने-आपको कामना में मिला देता है; किन्तु यदि अहं अपने-आपको कामना के साथ एक रूप होने का प्रयल करने के स्थान पर स्वयं का विवेक-शक्ति से तादात्म्य कर लेता है तो वह कहेगा, 'मुझे यह नहीं चाहिए।' लेकिन सामान्यतया अहं विवेकयुक्त नहीं होता, वह इच्छा के साथ अपने-आपको एक कर लेता है और विभिन्न इन्द्रियों को आज्ञाएँ देने लगता है। तुरन्त आप 'दूरभाष-निर्देशिका' में देखने लगते हैं और दुकान का फोन नम्बर खोजते हैं जहाँ वांछित वस्तु आप खरीद सकते हैं। यदि आप नम्बर पाने में सफल होते हैं, तो तुरन्त दूरभाष पर एक आर्डर दे डालते हैं। यदि आप दुकान का दूरभाष नम्बर नहीं ढूँढ़ पाते तो आप एक टैक्सी ले कर उस दुकान को जाते हैं और तब अनुभव एक बार पुनरोत्पादित हो जाता है। आप वहाँ बैठते हैं, मिष्टान्न प्लेट का आर्डर देते हैं और स्वाद लेते हैं। यह अनुभूति एक अन्य संस्कार छोड़ जाती है अथवा पुराने संस्कार को गहरा कर जाती है।
योग की प्रक्रिया संस्कारों को दग्ध करने की अपेक्षा करती है। एक बीज को पकाने वाले बरतन में रखिए और अग्नि में इसे तल दीजिए। अब यदि यह बीज मिट्टी में बोयें तो अंकुरित नहीं होगा; क्योंकि इसकी जीवनी-शक्ति पूर्णतया भून दी गयी है। यही बात समाधि में है। मैं आपसे केवल एक संस्कार के विषय में बात कर रहा हूँ जो कि इतना अधिक शक्तिशाली है। फिर यहाँ तो अगणित संस्कार होते हैं। जाने-अनजाने प्रतिदिन प्रातः से रात्रि तक हम उन ऐन्द्रिक अनुभूतियों को एकत्रित करते चले जाते हैं। प्रत्येक वस्तु जो हम अनुभव करते हैं, वह संस्कारों में परिणत हो जाती है। अपने जाग्रत जीवन के प्रत्येक क्षण में हम संस्कार ग्रहण करते जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि एक के बाद एक सभी संस्कारों को समाप्त करना असम्भव है। यदि एक परमाणु बम डाल दें तो हजारों मनुष्य एक ही साथ मारे जायेंगे। इसी प्रकार उन्होंने जो शस्त्र दिया, वह समाधि है-मनसातीत अवस्था है, जो कि एकबारगी समस्त संस्कारों को सदैव के लिए भून देगी जिससे कि वे उन अनुभवों को पुनरोत्पादित न कर सकें जिन्होंने मूलतः उन्हें जन्म दिया था। संस्कारों को विदग्ध करना योगियों की पद्धति है। इसे गहन ध्यान और संस्कार-नाश से उपलब्ध किया जाता है और मनुष्य बन्धन-मुक्त हो जाता है। यह योग की प्रक्रिया है। मन की खोज हेतु अग्रसरित होने पर उन्होंने जो खोजें कीं, यह उनमें से एक थी।
सम्पूर्ण राजयोग को मन के संस्कारों को विदग्ध करने की पद्धति कह सकते हैं।
२३. व्यावहारिक साधना-सकेत
दिव्य जीवनचर्या क्या है ?
योग-वेदान्त क्या है? दिव्य जीवनचर्या क्या है? योग-वेदान्त दिव्य जीवन का विषय है। दिव्य जीवन योग पर आधारित और वेदान्तिक भावना से ओत-प्रोत जीवन है और निःस्वार्थपरता, सेवा, साधना और आत्म-साक्षात्कार से निर्मित है। अतः योग और वेदान्त दिव्य जीवन का ताना-बाना या वह सामग्री है जिससे दिव्य जीवन बनता है। इसलिए स्वभावतः जितना ही अधिक हम इसके विषय में जानते हैं उतना ही अधिक हमें महत्त्वशील रूपों का स्मरण आता है और हम दिव्य जीवन यापन के लिए अधिक सम्पन्न होते हैं; क्योंकि दिव्य जीवन जीना जितना अधिक महत्त्वपूर्ण है, उतना इसके विषय में जानकारी करना नहीं। किन्तु जानने का महत्त्व इस सरल सत्य पर निर्भर करता है कि यदि आपको ऐसा जीवन यापन करना है तो आपको इसका कुछ ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। तभी इस ज्ञान के साथ आप अधिक सफलतापूर्वक इस जीवन में रहने योग्य होंगे। अतः ज्ञान भी आवश्यक है; किन्तु सर्वाधिक महत्त्व की बात है ऐसा जीवन यापन करना। योग के जीवन में, जो कि व्यावहारिक वेदान्त का जीवन है, हम कई विघ्नों के मध्य से गुजरते हैं और अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनका सामना हमें बुद्धिमत्ता से ज्ञानयुक्त हो कर करना पड़ता है और इसलिए इन विषयों की चर्चा तथा इन विषयों की जटिलताओं तथा सूक्ष्मताओं के बारे में सम्पूर्ण ज्ञान हमें एक अच्छी स्थिति पर पहुँचा देगा जिससे कि हम अपने योग और वेदान्त के जीवन में, दिव्य जीवन यापन के समय में, हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष आने वाली परिस्थितियों से निपटने योग्य हो सकें।
धर्मक्षेत्र
हमें कौन-सी बातें समझनी हैं? स्पष्टतः हमें योग और वेदान्त-सम्बन्धी वास्तविकताएँ समझनी हैं; क्योंकि इसी मार्ग के बीच में से हमें दिव्य जीवन यापन करना है और दिव्यत्व तक पहुँचना एवं आनन्द प्राप्त करना है। लेकिन तब हम योग और वेदान्त तथा सभी ऐसे अन्तरंग विज्ञानों का क्या अर्थ लेते हैं? वे कहाँ हैं? क्या वे केवल पुस्तकों में हैं अथवा वे विशिष्ट स्थानों जैसे हिमालय या उत्तरकाशी या मक्का या अन्यत्र हैं? मान लो वे वहाँ हैं। अगला प्रश्न उठता है-क्या वे केवल वहीं पर हैं और अन्यत्र कहीं नहीं ? अथवा इससे अधिक महत्त्व का प्रश्न यह कि क्या यह हमारे लिए आवश्यक है कि उनकी स्थिति का कहीं अन्यत्र भी पता लगायें ? वे एक रूप से पुस्तकों में हैं और दूसरे रूप में वे ऋषिकेश, मक्का जैसे स्थानों में हैं। ऐसे पवित्र तीर्थ-स्थानों में जाने का कुछ अर्थ है; क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों ने अपना जीवन व्यावहारिक व्यतीत किया है और उन्होंने अपने जीवन की छाप वहाँ उन स्थानों के वातावरण में अंकित की है। सम्पूर्ण वातावरण योग और वेदान्त की भावना से ओत-प्रोत है। अतः जब आप वहाँ रहते हैं, यह आपमें वही भावना जाग्रत करते हैं। किन्तु सर्वतोधिक महत्त्व का स्थान, जहाँ समस्त दिव्य जीवन, योग और वेदान्त का अभ्यास किया जाना है-धर्मक्षेत्र है, जो मनुष्य के मन और हृदय से निर्मित है। दिव्य जीवन मन और हृदय में यापन करना पड़ता है। योग को यहीं (हृदय के अन्दर) प्राप्त (पूर्ण) करना है। वेदान्त को यहीं प्राप्त (पूर्ण) करना है। यदि वह यहाँ नहीं है तो अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। वेदान्त और योग को हृदय और मन से आना है। आप अपने ज्ञान, भक्ति, निःस्वार्थ सेवा तथा योग को कैसे व्यक्त करेंगे? आपको इनका अभिव्यक्तिकरण अपने उन विचारों, शब्दों तथा कर्मों द्वारा करना होता है जो कि आप सोचते, बोलते या करते हैं। जब तक कि आप विश्व के शास्त्रों को अपनी व्यक्तिगत सत्ता द्वारा अभिव्यक्त न करें तब तक वे सब किसी उपयोग के न होंगे। साधना, वेदान्त, योग इस सम्पूर्ण विषय को जीवन में उतारना है। योग, वेदान्त और दिव्य जीवन के लिए सर्वाधिक महत्त्व का स्थल मनुष्य का अन्तस्तल है। अतः सर्वप्रथम प्रत्येक जीव को चाहिए कि अपने-आपको समझे। व्यक्ति को सर्वप्रथम इस रहस्यमय धर्मक्षेत्र को समझना चाहिए जहाँ इन सभी बातों का अभ्यास करना है। तब वह योग, वेदान्त और दिव्य जीवन के मार्ग में सही रूप में चलने योग्य हो सकेगा।
मन स्वर्ग-नरक का निर्माता है
आप चाहे जो कुछ भी हैं, अपने-आपसे पलायन नहीं कर सकते। यदि आप समझते हैं कि निवृत्ति का जीवन यापन करने के लिए पारिवारिक बन्धन बड़ा विघ्न है; आप परिवार को छोड़ सकते हैं। आप अपने घर या शहर से पलायन कर सकते हैं। ठीक है। आप एक अवधूत बन सकते हैं। आप पैन्ट, कोट छोड़ केवल एक कौपीन पहन सकते हैं। यदि आप समझते हैं कि मनुष्यों का संग अनुकूल नहीं है, आप उनका संग त्याग सकते हैं। वास्तव में अनेक लोग कसबों में प्राप्त कुसंगति से बचने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ भी वे बुरी संगति का असन्तोष व्यक्त करते हैं। यदि आप स्वयं रोटी बनाना नहीं चाहते तो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो रोटी बनाता हो। ठीक है, आप परिवार से, वस्तुओं से और लोगों के संग-साथ से पलायन कर जाइए, लेकिन विचित्र बात यह है कि आप अपने-आपसे पलायन नहीं कर सकते। इसका आशय क्या है? आपको अपनी जिह्वा, अपनी सभी इन्द्रियाँ अपने साथ ले जानी होंगी और अपनी इन्द्रियों के साथ-साथ उन आदतों को भी साथ ले जाना पड़ेगा, इन्द्रियाँ जिनकी दास हैं। यदि आप तम्बाकू के व्यसनी (लती) हैं तो आपको तम्बाकू का व्यसन, चाहे आप उत्तरकाशी चले जायें, वहाँ भी अनुभव होगा और इस प्रकार आप अपने साथ सभी इन्द्रियों को ले जाते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ आप अपनी समस्त आदतों और मन की प्रवृत्ति-विशेष को और राग-द्वेष, प्रेम और घृणा से युक्त अपने मन को अपने साथ ले जाते हैं।
दो विरक्त
एक बहुत सुन्दर कहानी है जो श्री गुरुदेव ने एक बार कही थी। दो अवधूत थे। वे महा-विरक्त थे। वे केवल एक कौपीन पहन कर रहा करते थे। शीतकाल में पराल (फूस) बिछा कर सोया करते थे और दोनों पराल रखा करते थे। उत्तरकाशी में धूप मिलना कठिन है और जहाँ भी धूप आती थी, वे पराल का बिस्तर ले जा कर रख दिया करते थे जिससे वह कुछ गर्म हो जाये। एक अवधूत जब अपना पराल का बिस्तर सुखा रहा था तभी दूसरा अवधूत, जो कि अपने में विचार-मग्न, किसी क्षेत्र से आ रहा था, उस पराल के बिस्तर पर पैर रखते हुए निकल गया। तुरन्त प्रथम अवधूत क्रोधित हो उठा और चिल्लाया, 'क्या तुम सूखने के लिए रखे गये इस पराल को नहीं देख सकते हो ?' मेरे-तेरे का विचार प्रवेश कर गया और वे एक-दूसरे को गाली देने लगे। यह कल्पित कथा नहीं है, बल्कि उत्तरकाशी में घटित वास्तविक घटना है।
वासनाओं का सफाया करो
स्वामी जी कहा करते थे कि केवल सिर का ही मुण्डन नहीं करना है, वरन् वासनाओं का भी करना है। अवधूत अपने निजी मन एवं वासनाओं के वशीभूत था। उसमें अहन्ता (ममत्व) का भाव था। यह भावना अपने-आपमें मन की जादूगरी ही है। हिन्दुत्व में 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' - प्रत्येक वस्तु अपने-आपमें ब्रह्म है, वहाँ कोई शैतान नहीं है; अन्य सभी धर्मों में ईश्वर भी है और शैतान भी है। ईसाई धर्म में शैतान है, पारसी धर्म में अर्हिमन है। लेकिन हिन्दू धर्म में सभी ब्रह्म हैं। तब शैतान कहाँ है? वह केवल मन में है। अतएव, आप चाहे उत्तरकाशी में रहें या मुम्बई में, आप अपनी इन्द्रियों और मन से नहीं बच सकते। जब तक आप यह नहीं जानते कि उनसे कैसे व्यवहार किया जाये, उनसे कैसे निपटा जाये, वे निरन्तर आप पर शासन करेंगे और आपसे सरसरी तौर पर व्यवहार करते रहेंगे और अन्ततोगत्वा आप पर क्या घटित होगा? आपकी विरक्ति और सभी बातें विलीन हो जायेंगी। कोई भी व्यक्ति जब तक अन्तस्तल में खोजबीन और आन्तरिक यन्त्र को समझने का प्रयास नहीं करता, वह साधना का अभ्यास सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। जहाँ भी आप जायेंगे, अन्तःमशीनरी साथ रहेगी। आप इसे मुम्बई में छोड़ कर यहाँ आ कर काम करें, ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि तब भी बिना मन के आप ईश्वर-चिन्तन नहीं कर सकते। बिना इसके आप धारणा और ध्यान नहीं कर सकते, बिना इसके स्मरण और चिन्तन सम्भव नहीं। बिना मन, भावनाओं, विचारों और अनुभूतियों के आप भाव एवं भक्तियुक्त नहीं हो सकते। अतएव, मन एका साधन है। यह अनिवार्य है और साथ ही यदि इसकी सम्यक् जानकारी और व्यवस्था न की गयी तो यह तुम्हारी करनी पर पानी फेर देता है। अतः यह एक अपरिहार्य अभिशाप है जिसे वरदान में परिणत करना है। अशुद्ध मन को कैसे पवित्र किया जाये ? इससे युद्ध करो, इसे दण्ड दो, दमन करो, पवित्र करो और शुद्ध मन में रूपान्तरित करो जिससे यह तुम्हारा मित्र बन जाये यह जप, कीर्तन आदि की भाँति किसी भी योग-क्रिया से कम नहीं है। प्रत्येक साधक को अपनी बुद्धि का प्रयोग और इन्द्रिय एवं मन से व्यवहार करने के महत्त्वशील कार्य से निपटना है। एक अनुशासनहीन वस्तु से आप निपट सकते हैं, परन्तु तभी जब आप उसको समझ लें। यदि घुड़सवार (अश्वारोही) घोड़े की आदतों को नहीं जानता तो उसका नियन्त्रण नहीं कर सकता। अतएव, यह साधना का एक अति महत्त्वपूर्ण भाग है।
मन क्या है!
अधिकांश लोग समझते हैं कि मन केवल विचार है। मन वह चीज है जिससे हम सोचते हैं, परन्तु मन कुछ इस प्रकार का सरल नहीं है। चाहे आप विचार न करना चाहें तो भी मन सामान्यतः सोचता है। यह पदार्थों के विषय में सोचता है। विद्यालय में एक अति-गर्म और उमस वाला दिन था। अकस्मात् एक लड़का थक गया और वह ऊब गया। उसने तेज सीटी बजा दी। अध्यापक ने जब उससे प्रश्न किया कि उसने ऐसा क्यों किया तो लड़के ने उत्तर दिया, 'मैंने सीटी नहीं बजायी, वह अपने-आप बज गयी।' इसी प्रकार प्रत्येक मिनट मन अपने-आप अपनी विचारधारा को सोच रहा है। जहाँ तक मन विचारोत्पादन में संलग्न है, वह एकाग्र नहीं हो सकता। इसे आपको ईश्वर की ओर घुमा देना है। लेकिन यह कैसे किया जाये ? मन क्यों इधर-उधर भटकता फिरता है? साधक को यह सब समझना है। एक कर्मयोगी को इसे समझना है, एक भक्तियोगी को इसे समझना है।
आप चाहे अकेले हों या लोगों के मध्य में, आपको इसे समझना है। दूसरी ओर, जब आप अकेले होते हैं, मन को अपना पूर्ण नाटक दिखाने का एक अवसर मिलता है। यह रहस्यात्मक चीज क्या है जो साधक के लिए ऐसी समस्या है जिसके बिना वह साधना नहीं कर सकता; किन्तु साथ ही यदि यह नियन्त्रित न की गयी तो साधक को पतनोन्मुख कर देती है। मन कैसे कार्य करता है? यदि हम इसके स्वभाव का मौलिक ज्ञान प्राप्त कर लें, तब हम इस पर नियन्त्रण-प्राप्ति के कुछ साधन निर्देशित कर सकेंगे।
मन की पद्धतियाँ
मन विभिन्न रहस्यात्मक पद्धतियों से कार्य करता है। हम इस मानसिक प्रक्रिया के कुछ महत्त्वपूर्ण विशद रूपों का विश्लेषण करेंगे। किसी विशेष क्षण में एक व्यक्ति का मन क्या होता है? मन किससे बना है? इसे मैं कुछ सरल सादृश्यों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न करूँगा। सर्वप्रथम आप दो तुलनात्मक सादृश्य लें। आप एक ग्रामोफोन का रेकार्ड लें। यह किससे बना है ? साधारणतः आप एक रेकार्ड देखते हैं और आप देखते हैं कि यह पतली धारियों से बना है-रेखाओं से पूर्ण है। एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए यह इससे अधिक कुछ अर्थ नहीं रखता। कुछ अधिक बुद्धिमान् और शिक्षित व्यक्ति कहेगा, यह रेखाओं से युक्त है और ये रेखाएँ गुप्त रूप से ध्वनियाँ हैं। कुछ और अधिक बुद्धिमान् व्यक्ति कुछ अन्य बातें कहेगा। वह कहेगा कि प्रत्येक धारी विशिष्ट ध्वनि रखती है। यह कार्य रूप में है। यह ध्वनि उस ध्वनि से, जो सृजनात्मक (कारण) थी, एक समान है। कुछ अत्यधिक बुद्धिमान् और विद्वान् पुरुष बता देगा कि कौन-सी विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं जिनमें यह ध्वनि उत्पादित (प्रकटित) करेगी।
एक दूसरा सादृश्य लें। तुम एक बीज लो। एक शिशु कहेगा कि यह बहुत छोटी वस्तु है, लेकिन अधिक विचारशील मस्तिष्क वाला एक कवि कहेगा, 'आपके हाथ में उच्च बलूत वृक्ष है, जो एक सहस्र लोगों को शरण दे सकता है।' कुछ और अधिक योग्य व्यक्ति कहेगा, 'यह बीज एक बलूत वृक्ष पैदा कर सकता है। यह उसी प्रकार का बलूत पैदा कर सकता है जिससे यह प्रसूत है। और केवल इतना ही नहीं, यदि वह वृक्ष भविष्य में बीज पैदा कर सकता है तो इसका अर्थ हुआ कि यह अपने में पुनरारम्भ की और एक बार पुनः सम्पूर्ण क्रिया के अभिव्यक्तिकरण की क्षमता रखता है जो कि इसमें पूर्व हो चुकी है।' अतएव यह एक सजीव वस्तु है, एक गतिशील वस्तु है। यह अपने-आपमें सम्पूर्ण चक्र रखता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का मन निर्दिष्ट समय में अपने अन्दर में शब्दों के अन्दर शब्द रखता है। इस वस्तु का स्वरूप ग्रामोफोन रेकार्ड पर की धारी अथवा बीज के स्वरूप का है। यह बीज क्या है ? ये धारियाँ (रेखाएँ) क्या हैं जो मन में हैं? मन अनुभव, पूर्ण अनुभव की उपज है। ठीक उसी प्रकार यह अनुभवों की उपज किस प्रकार है? हम अभी एक उदाहरण लेंगे और हम उसको अनन्त गुणन कर सकते हैं।
प्रच्छन्न वासनाएँ
यह एक अनुभव है। यह अनुभव एक इन्द्रियानुभूति के रूप में हो सकता है। आप कुछ सूंघते हैं, कुछ स्पर्श करते हैं, कुछ रसास्वादन करते हैं, अथवा अनेक वस्तुओं का मिश्रित अनुभव करते हैं और तुरन्त जैसे ग्रामोफोन के रेकार्ड में ध्वनि की प्रबलता से एक रेखा खिंच जाती है, उसी प्रकार मन में भी एक अनुभव प्रस्थित हो जाता है। यह अनुभव ही संस्कार कहलाता है जो कि इन्द्रियजन्य अनुभव का मन में प्रभाव ही है। संस्कारों का स्वरूप क्या है? क्या यह भूमि पर बनी रेखाओं के समान है या ग्रामोफोन रेकार्ड में बनी धारियों के समान है? नहीं, यह गतिशील है और ऐसे अनेक अनुभव मानव-मन में रेकार्ड की रेखाओं के समान गहरे और जीवन्त प्रभाव डाल जाते हैं। यह सक्रिय हो जाता है। मनुष्य के जीवन में यह तत्त्व प्रगतिशील होना प्रारम्भ हो जाता है। अर्थात् व्यक्ति के चरित्र में यह गतिशील प्रवृत्ति का रूप ले लेता है और जब यह इस स्थिति पर आ जाता है तो किसी विशिष्ट प्रभाव को बार-बार ग्रहण करने से यह शक्तिशाली एवं सजीव शक्ति का रूप मनुष्य के चरित्र में धारण करवा देता है। यह साधक के चरित्र में विशेष गुण हो जाता है। यही वासना कहलाती है। इसका अर्थ हुआ कि प्राणी का सदैव उस दिशा की ओर क्रियाशील होने का झुकाव रहता तथा सदैव उस प्रेरणा के अनुसार व्यवहार करने की प्रवृत्ति रहती है। इस प्रकार संस्कार जब दोहराये जाते हैं तो वासना बन जाती है और ये वासनाएँ सदैव मन को उद्वेगावस्था में रखती हैं तथा वे सदा मन-रूपी झील में हिलोरें (तरंगें) पैदा करती रहती हैं जो कि वृत्तियाँ कहलाती हैं।
वृत्तियाँ
अतएव साधारण मन में अनेकानेक वृत्तियाँ उठती और डूबती हैं। जब वृत्तियाँ मन में उठती हैं तो व्यक्ति श्रेणीबद्ध कल्पनाएँ प्रारम्भ कर देता है। आप एक कल्पना का प्रारम्भ करते हैं। यदि कल्पना वहाँ न हो तो वृत्तियाँ मनुष्य को कष्ट न देंगी। जब वृत्तियाँ सृजनात्मक कल्पना का सहारा पाती हैं तो वे कामना (इच्छा) का रूप धारण कर लेती हैं। इस इच्छा का, जो कि कल्पना के बल से निर्मित है, स्वरूप क्या है? यह उसी अनुभव के किस्म की है जिसने संस्कार उपजाया था, जो पुनः वृत्ति के उठने का कारण या हेतु बन गयी। यहाँ इच्छा की इस स्थिति तक कोई अधिक हानि नहीं है, लेकिन जब हममें से प्रत्येक में अहंकार का खेल, 'मैं' उस इच्छा के साथ स्वयं को सादृश्य कर लेता है, वहीं से समस्त झंझट प्रारम्भ हो जाता है। बजाय 'आवश्यकता' के यह 'मुझे आवश्यकता है' का रूप धारण कर लेता है। अब व्यक्ति मन की पकड़ में आ गया। चाहे आप एक गुफा में रहें या एक नगर में, जब 'मैं' और 'कल्पना' दोनों जुड़ जाते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि 'मुझे बातचीत की आवश्यकता है, मुझे एक सिगरेट की आवश्यकता है।' जब इच्छा अहंकार के साथ सादृश्यता को प्राप्त हो गयी, तब सभी झंझट उठ खड़े होते हैं। चाहे आप ध्यान ही कर रहे हों, किन्तु जब आप किसी विशेष वस्तु की इच्छा करते हैं तो ध्यान गौण हो जाता है। आप कामना-पूर्ति हेतु इधर-उधर चले जाते हैं, लेकिन तब भी मन के दो पक्ष होते हैं। जब कोई इच्छा उठती है तो मन सोचता है, मुझे इस कामना की पूर्ति करनी चाहिए या ध्यान ही लगाये रहना चाहिए? क्या मुझे जा कर इडली लेने में समय व्यर्थ नष्ट करना चाहिए? अब वहाँ विचार होने लगता है। यदि सही निर्देशन है तो शुद्ध मानस विजयी होता है। यह कहता है, 'नहीं' और यह इच्छा को ढकेल (धक्का) देता है और ध्यान का नैरन्तर्य बनाये रखता है। दूसरी ओर यदि अशुद्ध मानस को प्रश्रय दे देता है तो इच्छा विजयी होती है। तब इच्छा तृष्णा बन जाती है और इस तृष्णा से क्या घटित होता है? व्यक्ति तुरन्त इच्छा की पूर्ति हेतु प्रयास करता है और योग से भ्रष्ट हो जाता है।
इच्छा की प्रक्रिया
योग निर्विकल्प समाधि में ही नहीं है। यह प्रत्येक क्षण का है। यदि एक विचार आता है और आप इसको दमन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप योग में असफल हो गये, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये। प्रत्येक विचार में, प्रत्येक क्रिया में आपको अपनी वृत्तियों पर स्वामित्व बनाये रखना है। तभी योग पूर्ण होता है, दिव्य जीवन यापन होता है। इस प्रक्रिया में कितना समय लगा? यह एक क्षण-भर का है। एक सेकेण्ड के अंश मात्र में अनेक चित्र (भाव) चित्रित होते चले जाते हैं। यही बात मन के साथ है। समस्त प्रक्रिया संस्कार से प्रारम्भ हो कर चेष्टा या इच्छा-पूर्ति की समाप्ति तक एक सेकेण्ड के अंश मात्र में सम्पन्न हो जाती है। अनुभूति से आप संस्कार पाते हैं, संस्कार से वासना पाते हैं और वासना से आपकी वृत्ति बनती है। तब कल्पना वृत्ति को इच्छा में निर्मित करती है। तब अहं अपने-आपको इच्छा से संलग्न करता है और तब यह एक तृष्णा बन जाती है। तब आप चेष्टा या इच्छा-पूर्ति के लिए विवश हो जाते हैं। मन की यह प्रक्रिया चलती रहती है।
मन-सनातन मशीनरी
वैज्ञानिक ऐसी मशीनरी की प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर रहे हैं जो निरन्तर चलती रहे, कभी रुके नहीं, बल्कि सदैव गतिशील रहे। यदि आपको निरन्तर गतिशील मशीनरी खोजनी हो तो यह आपके अन्दर 'मन' है। हमें मन के साथ व्यवहार करना होता है। समस्त वासनाएँ, संस्कार जो हमने बनाये हैं, पहले से वहाँ हैं। यद्यपि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते; पर कम-से-कम एक बात तो कर ही सकते हैं और वह यह कि हम नवीन संस्कारों का बनना रोक दें तथा पूर्व-संस्कारों को भी भविष्य में ताजे संस्कारों द्वारा दृढ़ न होने दें। यह कैसे सम्भव है? प्रतिदिन हम नवीन संस्कारों को ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन हम अनेक वस्तुओं को अपनी पंच-ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। तब हम इन अनुभवों को मन में अनुभूतियाँ अंकित करने से कैसे रोक सकते हैं? क्या कोई प्रविधि है? ये वस्तुएँ कैसे मन में प्रवेश करती हैं और संस्कार बना देती हैं? (विचारार्थ) एक वस्तु को लें। अपनी इन्द्रियों में से किसी एक के द्वारा आप इसे ग्रहण करते हैं। प्रथमतः इन्द्रिय और वस्तु के बीच में सम्पर्क होता है। यह प्रथम बात है। फिर क्या होता है? अभी तक मनुष्य के व्यक्तित्व का केवल बाह्य अंचल ही स्पर्श किया गया है। मान लो आप किसी कार्य में गम्भीरता से मग्न हैं और आपका अनुज या अनुजा आती है और अपने हाथ आपके ऊपर फैला देती है। आपको भान नहीं होता, क्योंकि वस्तु ने केवल इन्द्रिय से सम्पर्क किया है; किन्तु इन्द्रिय ने इसे मन को सम्प्रेषित नहीं किया है, क्योंकि मन इससे दूर है। वस्तु ने इन्द्रियों से सम्पर्क किया और इन्द्रियों ने इसे मन को सम्प्रेषित किया; लेकिन यदि आप वहाँ नहीं हैं, यदि 'मैं' का भान वहाँ नहीं है तो मन के द्वारा प्राप्त अनुभूति, नित्य परिपाटी के समान, व्यक्ति के लिए कोई अर्थ नहीं रखती। अतः यदि अहंकार वहाँ नहीं है तो वस्तु मन (अन्तःकरण) की गहराई तक नहीं प्रवेश करती। यदि अहं किसी अन्य विचार में व्यस्त है तो इन्द्रियों द्वारा ग्रहीत विशिष्ट अनुभूति किंचित् भी प्रभावोत्पादक नहीं होगी; लेकिन यदि 'मैं' वहाँ है, तो वस्तु प्रविष्ट हो जाती है और आपके सचेतन मन पर टक्कर मारती है। यदि यह 'मैं' असावधानी की अवस्था में है, सचेतन नहीं है, अबिवेक की अवस्था में है अथवा सांसारिकता की दशा अथवा रजस् में है तो वह सरलता से इन इन्द्रियानुभूतियों को ग्रहण कर लेगा और आपमें वस्तुओं के लिए एक इच्छा उत्पन्न कर देगा।
इच्छाओं को भस्मसात् करें
यदि आप सावधान, वैराग्यपूर्ण और आत्मत्यागी नहीं हैं तो जिस क्षण वस्तुगत स्मृति आपमें उदय हुई, आप उस वस्तु के पीछे दौड़ पड़ते हैं। मनुष्य धन देखता है और तुरन्त ही इसकी कामना करने लगता है। मान लें कि वह अजेय स्थिति तक पहुँच गयी तो बचाव का केवल एक ही मार्ग है। आप क्या कर सकते हैं? आप केवल उस इच्छा में दियासलाई लगा कर उस इच्छा को जला दें। उस इच्छा को राख कर दें। लेकिन कैसे ? समस्त इच्छाओं को जला देने की केवल एक अग्नि है। नचिकेता के पास वह अग्नि थी। यम ने इतनी अधिक आकर्षक और लुभावनी वस्तुओं का प्रस्ताव रखा। उसने धन, सुन्दरता, ताकत, शक्ति, साम्राज्यों और समस्त विश्व तथा समस्त विद्याओं के स्वामित्व तक का प्रस्ताव रखा। यम ने समस्त आकर्षक और लुभावने संसार के रोचक वर्णन प्रस्तुत किये, लेकिन नचिकेता ने उन सब इच्छाओं को भस्म कर डाला; क्योंकि उसके पास एक अग्नि थी और वह थी मुमुक्षुत्व की अग्नि। मुमुक्षुत्व एक सकारात्मक अग्नि है जिसमें समस्त इच्छाएँ डाल दी जाती हैं और भस्मसात् कर दी जाती हैं। यही अग्नि है जो समस्त साधकों, योगियों, वेदान्तियों और दिव्य जीवन यापन करने वालों की विशिष्टता बतलाती है।
सच्चे शिष्य बनो
गुरुदेव स्वामी शिवानन्द के शिष्य में उत्कट इच्छाग्नि होनी चाहिए। तभी वह गुरुदेव का वास्तविक शिष्य है। यदि हम अपने को गुरुदेव स्वामी शिवानन्द के सच्चे शिष्य कहलाना चाहते हैं तो हमसे यह आशा की जाती है कि हम ऐसे महर्षि के शिष्यत्व के विशिष्ट गुणों और लक्षणों को मन में स्मरण रखें। ऐसे शिष्यत्व का मुख्य एवं सामान्य विशेष गुण यह ज्वलन्त उत्कट इच्छा की अग्नि ही है। यदि आप दिव्य जीवन यापन करना चाहते हैं तो आपका अन्तर-हृदय उत्कट अभिलाषा-स्थली होना चाहिए। योग की अग्न्नि आपके अन्तर में सदैव प्रज्वलित रहनी चाहिए। अग्नि की यह लपट वहाँ होनी चाहिए। आप जीवन की बाह्य पद्धति को पूर्णतया परिवर्तित नहीं कर सकते; किन्तु अन्तर में उत्कट इच्छा होनी चाहिए। जब आप अकेले हों, जब आप लोगों के बीच में हों, जब आप ध्यान में हों, जब आप कार्य में व्यस्त हों, यह अग्नि अहोरात्र प्रज्वलित रहनी चाहिए। यह अग्नि प्रशमित नहीं होनी चाहिए। यह उत्कट इच्छा सदैव आपके आन्तरिक अंग के रूप में होनी चाहिए। तभी आप दिव्य जीवन यापन कर रहे होंगे। यदि यह अग्नि वहाँ है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, किस स्थान में आप रह रहे हैं; क्योंकि आप दिव्य जीवन यापन कर रहे होंगे। आप विषय-भोगों के शिकार नहीं होंगे, लेकिन आपको सदा यह ज्ञात रहना चाहिए कि आपकी सावधानी के बावजूद यदि कोई विषय आपकी अन्तश्चेतना में प्रवेश करता है तो उत्कट इच्छा के द्वारा कैसे उसे भस्मसात् कर दें? इसकी दो प्रविधियाँ हैं- प्रत्याहार और उदासीनता। प्रथम प्रविधि है मन को सदैव अन्तर्मुखी बनाये रखना। मन को पूर्णतया कभी भी बहिर्मुखी न होने दें जिससे कि बाह्यतः चाहे आप विषयों के मध्य विचरण कर रहे हों, इन्द्रियाँ बहिर्मुखी न हों, वे अन्तर्मुखी रहें। यह अति-क्लिष्ट विशिष्ट विद्या है, लेकिन इसका अभ्यास करना ही है। यह प्रत्याहार अत्यावश्यक है। यह अति-क्लिष्ट और विशिष्ट विद्या है, लेकिन इसे पूरा करना सम्भव है। साधक का आदर्श सदैव इस महत्त्वपूर्ण प्रत्याहार की योग्यता को प्राप्त करने का होना चाहिए।
मन की उदासीनता
द्वितीय पद्धति है पदार्थों के प्रति उदासीनता। इसका आपके लिए क्या अर्थ है? आपके लिए इसका कोई भी मतलब न होगा। यदि एक मांसाहारी व्यक्ति बाजार में जाता है, जहाँ मछली, मुर्गी आदि का मांस विक्रय होता है तो उसके मुँह में पानी आ जायेगा। लेकिन कल्पना करो कि वह व्यक्ति शाकाहारी है और वह वहाँ जाता है तथा इन पदार्थों को देखता है। उसके लिए इन पदार्थों का कोई मतलब नहीं, वह इनसे सरोकार नहीं रखता। इसी प्रकार हमें अपने-आपमें सतत मनन से संसार की निस्सारता, भौतिक पदार्थों की व्यर्थता और सम्पूर्ण सृष्टि की क्षणभंगुरता का दिग्दर्शन कराने वाले शास्त्रों के सतत स्वाध्याय से एक प्रवृत्ति उत्पन्न करनी होगी। ऐसे विचारों को सतत आत्मसात् करने से मन का एक स्वभाव उत्पन्न होता है, जब आपके लिए समस्त पदार्थों की अर्थवत्ता समाप्त हो जाती है और तब चाहे ये पदार्थ सामने आयें, फिर भी अन्दर से कोई उत्तर यानी ग्रहण-भाव नहीं होता। यह स्थिति उदासीनता कहलाती है। आप साधारणतया ही कोई अभिरुचि नहीं रखते और जब एक वस्तु को पसन्द नहीं करते तो आप इसमें अभिरुचि नहीं रखेंगे। लोग जिस पदार्थ को पसन्द नहीं करते, उसके सम्बन्ध में उनका यही अनुभव है। जब कभी वे कोई पदार्थ देखते हैं जिसे वे पसन्द नहीं करते, वे उसमें अभिरुचि नहीं रखते। पदार्थ में अभिरुचि न रखने की इस प्रवृत्ति को व्यापक बनाना चाहिए। एक साधक जब पदार्थों के मध्य में हो तो उसे उदासीनता की यह अभिवृत्ति रखनी चाहिए। यह आदत उत्पन्न करनी चाहिए। यह प्रविधि प्रत्याहार की भाँति नहीं है, बल्कि मन की यह प्रवृत्ति शनैः-शनैः विकसित की जाती है और इसकी गहराई की मात्रा भी वर्धित की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्याहार और उदासीनता से हम पदार्थों को इन्द्रियों से अधिक प्रारम्भिक संसर्ग की अवस्था में जला (विनष्ट कर) सकते हैं। यदि आपको पदार्थों के मध्य रहना है तो आप इन दो पद्धतियों से पदार्थों के संसर्ग को काट सकते हैं। लेकिन यदि उसके बावजूद इन्द्रियानुभूति सीधे आपके अन्तर-प्रकोष्ठ में प्रवेश करती है, तो उत्कट महत्त्वाकांक्षा की अनि द्वारा इसे अस्वीकार (प्रत्यादेशित) कर दें, जला दें। इस प्रकार आपको संसार में विचरण करना है। आपको यह साधन रखना चाहिए।
मन को किसी वस्तु पर केन्द्रित रखिए
एक सकारात्मक पद्धति भी है। आप विश्व से सभी पदार्थ हटा नहीं सकते। आप विश्व से सभी लोगों को हटा नहीं सकते। आपको विश्व में रहना है। अतः एक अति-रुचिकर पद्धति प्रस्तुत करते हैं। एक सन्त का कथन है कि यदि आप काँटों-भरे जंगल से गुजरना चाहते हैं तो सुरक्षित चल पाने की व्यवस्था की दृष्टि से आप जंगल की भूमि को गलीचे से नहीं ढक सकते। समस्त जंगल को ढकने का प्रयास करने के बजाय एक बुद्धिमान् मनुष्य एक जोड़ी चप्पलें पहन लेगा। यह उतना ही उपयोगी होगा जितना कि समस्त जंगल को गलीचे से ढक देना; क्योंकि जहाँ-कहीं भी वह जायेगा, यह सुरक्षा उसके साथ होगी। उसी प्रकार हम विश्व को पूर्णतया विलीन नहीं कर सकते, किन्तु हम अपने-आपकी रक्षा इस प्रकार कर सकते हैं कि हम संसर्ग से प्रभावित न हों और इस प्रकार प्रत्याहार और उदासीनता के माध्यम से हमें अपने-आपकी उन पदार्थों से रक्षा करनी है जो हमारे मन में संस्कार पैदा करते हैं और सकारात्मक पद्धति यह है : सदैव मन को किसी वस्तु पर केन्द्रित रखिए। यदि आपको किसी दुर्गन्धयुक्त स्थान से हो कर जाना है तो आप सभी स्थलों पर कोई सुवासित चीज नहीं छिड़कते; किन्तु यदि आप नाक में कस्तूरी निर्मित इत्रयुक्त कोई पदार्थ रख लें तो आप सदैव कस्तूरी की सुगन्ध का अनुभव करेंगे, आप दुर्गन्ध नहीं अनुभव करेंगे। इसी प्रकार से आप सदैव भगवन्नाम का मानसिक जप और नाम-स्मरण करें और कतिपय महान् आदर्श स्मृति में रखें। वेदान्ती महावाक्य के सतत जप के साथ कहेंगे, 'सब ब्रह्म है, सच्चिदानन्द है।' भक्त अपने इष्टमन्त्र के साथ कहेंगे, “सब राम या सब कृष्ण है।' मन के लिए ये बातें सकारात्मक आधार हैं जिनमें कि मन अनुरक्त हो सके। इस प्रकार मन की अन्य पदार्थों की ओर जाने की प्रवृत्ति न्यून हो जाती है; क्योंकि इसको एक धुरी दी जाती है जिसे यह पकड़े रह सके।
इच्छाओं से तद्रूपता दूर करें
यह सामान्य समझदारी की पद्धतियाँ हैं जिन्हें योगमय जीवन और व्यावहारिक वेदान्त का जीवन यापन करना चाहने वाले मनुष्य को साधना या सामग्री के रूप में रखना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया है, हम अपनी इन्द्रियों और मन से पलायन नहीं कर सकते।
अतएव, हमको मन की कार्यविधि समझनी चाहिए। जब कभी कोई वृत्ति उठने लगे तो इसके विषय में कुछ सोचें ही नहीं, इसको पूर्ववत् लय हो जाने दें। कल्पना भी न करें। कल्पना ही इसे सुदृढ़ बनाती है। इच्छा के साथ अपने-आपको एक-रूप न कीजिए और यदि इच्छा निकृष्ट से निकृष्टतर स्तर पर उतर कर बलवती हो उठती है तो जिद्दी या हठी बन जाइए। इसको प्रकट न होने दीजिए। गुरुदेव ने सदैव कहा है, "इच्छा के अंकुरित होते ही उसे तत्काल समाप्त करने का सदैव प्रयत्न कीजिए। जब एक इच्छा लघूर्मि के रूप में आये तो स्वतः इसे तुरन्त जहाँ की तहाँ मिटा डालने का प्रयत्न करें। लेकिन यदि आपकी सावधानी के अभाव के कारण यह एक इच्छा का रूप धारण कर ले तो देखिए कि इसकी सन्तुष्टि नहीं की जाती है। इसके लिए बाह्य चेष्टा न करें। यदि ऐसी इच्छा उठे कि 'मैं जाऊँ और गपबाजी करूँ' तो कहो, 'नहीं, मैं शरीर को हिलने की स्वीकृति नहीं दूंगा।' यदि शरीर नहीं हिलता तो मन विवश हो जाता है और अन्ततोगत्वा विपरीत प्रक्रिया घटित होगी और इच्छा मन में विलीन हो जायेगी तथा वहाँ शान्ति हो जायेगी।
मनोनिग्रह हेतु साधना
साधना के प्रारम्भ में भौतिक स्तर पर, अधिकाधिक इच्छाओं का नियन्त्रण करना होगा, किन्तु जैसे-जैसे हम अपने-आप पर स्वामित्व प्राप्त करते जायेंगे, तब कोई वृत्ति भी आती है तो वह भी लीन हो जाती है। ऐसा विचार और विवेक से किया जाता है। यह विचार और विवेक साधक के सहायक हैं। जैसे ही कोई वृत्ति उठती है, यह वापस कर दी जाती है और अन्ततोगत्वा भगवन्नाम के जप, ध्यान, प्रार्थना एवं पुरश्चरण-अनुष्ठान द्वारा इन सभी को पूर्णतया विनष्ट कर देना होता है। ये सभी शक्तिशाली सकारात्मक पद्धतियाँ हैं; क्योंकि वृत्तियाँ और संस्कार अगणित हैं और गहरे मूल तक हैं, किन्तु योगाभ्यास और सच्ची लगन से वे पूर्णतया विनष्ट कर दिये जाते हैं। साधक के मार्ग में अवरोधात्मक समस्त वासनाएँ जप, कीर्तन, प्रार्थना, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा पूर्णतया लय कर दी जाती हैं। अन्ततः मिश्रित पद्धतियों से यह कार्य सम्पादन किया जाता है, लेकिन उसी समय विवेक और विचार के द्वारा हमें मन से भी निपटना पड़ता है जिससे कि मन को इच्छा का रूप धारण करने का कभी अवसर न मिल सके।
मन का अध्ययन करें
इस प्रकार से हम जितना अधिक मशीनरी को समझते हैं, उतना ही अधिक हम इसकी समस्त सूक्ष्म चालों, अन्तरधाराओं सहित इससे व्यवहार करने योग्य होंगे और मन को अपने अन्तर में बजाय निरन्तर अवरोध क साधना के प्रभावी अस्त्र के रूप में प्रयोग करने योग्य होंगे। साधक का समस्त सर्वश्रेष्ठ आदर्शमयी स्थितियाँ प्रदत्त की जा सकती हैं। वह आदर वातावरण, आदर्श संगति तथा समस्त ग्रन्थों से युक्त हो सकता है, फिर भी यदि वह मन के कार्य करने के इस रहस्यमय स्वभाव को समझने के प्रयास का महत्त्वपूर्ण कार्य और वासनाओं को क्षीण करने और अपनी इच्छा-शक्ति को बलवती करने का प्रयास नहीं करता है तो वह (उपर्युक्त) किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता है। वह अपने गुरु से भी लाभ नहीं उठा सकता और न ही अपने एकान्तपन का उपयोग कर सकता है; क्योंकि इन सभी का उपयोग मन के माध्यम से ही किया जा सकता है और यदि मनोनिग्रह तथा मन का संस्करण नहीं किया गया तो वह इन सबका उपयोग नहीं कर सकता है। किन्तु यदि एक बार ऐसा कर लिया तो वह ईश्वर-प्रदत्त समस्त पदार्थों का उपयोग कर सकेगा। धर्म-ग्रन्थ का एक ही वाक्य उसके अन्तर में आध्यात्मिक चेतना की बाढ़ उत्थित करने में सक्षम होगा। अतः मन को समझें, मन का अध्ययन करें और उसकी मशीनरी का ज्ञान अच्छी तरह प्राप्त करें। इसको व्यवस्थित कैसे करें, यह भी जानिए। यह योग का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, वेदान्त का एक महत्त्वपूर्ण अंग है और साधना तथा दिव्य जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति के प्रारम्भिक अभ्यास में ये सभी महत्त्व के हैं। जब कोई इन सभी का अभ्यास कर लेता है तो ईश्वर-साक्षात्कार सरल हो जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर-साक्षात्कार करना बड़ा सरल है, इतना सरल कि फूल निचोड़ने में जितना समय लगता है उतने समय में यह प्राप्त किया जा सकता है। एक बार यदि आप मलिनताओं से पूर्ण छुटकारा पा गये तो आप उत्तम अधिकारी बन गये। उसके लिए हमें धैर्यपूर्वक कार्य करना है और जितना ही समय हम विनम्रता, सच्चाई और लगन के साथ अपनी निजी सत्ता और अपने अन्दर की इस मशीनरी-मन के अध्ययन हेतु लगाते हैं तथा इस यौगिक अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने में ध्यान देते हैं, उतना ही अधिक हम योग एवं वेदान्त के पथ पर बढ़ने में तथा दिव्य जीवन यापन में सफल होने योग्य होते हैं।
उच्च (परा) तथा निम्न (अपरा) मन
हमने अवलोकन किया कि किस प्रकार दिव्य जीवन यापन और समस्त यौगिक क्रियाएँ तथा व्यावहारिक वेदान्त मौलिक रूप से मन में ही घटित होते हैं। बाह्यतः ये प्रक्रियाएँ, जो अन्दर होती हैं, अपना संस्कार रखती हैं। वे व्यक्ति के कुछ व्यवहारों को रोकने और उसकी बाह्य प्रभावों की प्रतिक्रिया, जिन कार्यों में वह संलग्न रहता है उनकी प्रतिक्रिया के रूप में अपने-आपको व्यक्त करती हैं, किन्तु मूलतः वे अन्दर के कुरुक्षेत्र, मन में घटित होती हैं। निम्न जन्मजात प्रवृत्तियों और उच्च आध्यात्मिक आकांक्षाओं के मध्य, मन के उस भाग से जो इन्द्रियों को बाहर खींचता है, जो कि रजस् और तमस् से पूर्ण है तथा मन के सात्त्विक भाग-विवेकयुक्त बुद्धि, विचारयुक्त मानस, मन जहाँ ज्ञान-अज्ञान व्यक्त होना प्रारम्भ होता है, जहाँ मानव की चुनाव करने की बुद्धि ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है, उनके मध्य स्थायी संघर्ष मन में चला करता है। यह चयन करना प्रारम्भ कर देता है कि कौन उचित है तथा कौन अनुचित है, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, व्यक्ति की प्रगति के लिए क्या सहायक है और क्या हानिकर है? जब ऐसा नीर-क्षीर-विवेकी मन कार्य करना प्रारम्भ करता है तो मनुष्य वस्तुओं के सम्बन्ध में क्यों और किस लिए के प्रश्न पर विचारना प्रारम्भ कर देता है। यह नीर-क्षीर-विवेक सत्संग से या क्लिष्ट अनुभवों, जीवन की ठोकरों और धक्कों से अथवा पूर्व-संस्कारों के विकसित होने से अथवा नीर-क्षीर-विवेकी मन को जाग्रत करने वाले अगणित कारणों में से एक से उद्भूत होता है। पदार्थों की इच्छाओं से पूर्ण सहज प्रवृत्ति वाला मन मनुष्य को पतन की ओर कर्षित करने का प्रयत्न करता है, जब कि उच्चतर मन उसको ऊपर की ओर कर्षित करता है। अन्ततोगत्वा मनुष्य का आध्यात्मिक अंश ही सत्ता के निम्न सहज ऐन्द्रिक भाग पर अपनी निजी श्रेष्ठता स्थापित करता है और उसे आत्म-चेतना में पूर्णतया प्रतिष्ठित कर देता है जो कि योग की अन्तिम स्थिति है। इस प्रक्रिया में हमने अवलोकन किया कि मन किस प्रकार कार्य करता है, यह किस प्रकार व्यक्ति को बारम्बार अपने अनुभव, संस्कार, वासना, कल्पना, अहंकार, इच्छा, कामना और चेष्टा के दुष्ट चक्र में फाँसने का प्रयत्न करता है। जब आप चेष्टा करते हैं तो आप पुनः अनुभव की पुनरावृत्ति करते हैं जिससे एक संस्कार निर्मित होता है। संस्कार से वासना उत्पन्न होती है। वासना एक वृत्ति बन जाती है जो कल्पना की सहायता ले कर एक इच्छा बन जाती है। इच्छा अहंकार की सहायता लेती है और कामना बन जाती है और कामना वर्धित हो कर तृष्णा बनती है और तृष्णा के पश्चात् चेष्टा या पूर्ण (सन्तुष्ट) करने की वास्तविक इच्छा होती है और पुनः आनन्द-भोग संस्कार को दृढ़ करते हैं और इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया की बारम्बार पुनरावृत्ति होती है।
पुनरावृत्ति से संस्कार दृढ़ होते हैं
अतः इससे एक सत्य सम्मुख आता है। यदि एक इच्छा उठे और यदि आप उसे पूरा कर दें तो वह संस्कार, जिसने उस इच्छा को जन्म दिया, और अधिक दृढ़ हो जाता है। अतः साधकों को एक महान् सत्य स्मरण रखना है कि इच्छा को पूर्ण करने से इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। आप कभी भी इच्छाओं का अन्त उनको पूर्ण करते रह कर नहीं कर सकते। जिस प्रकार अग्नि की क्षुधित ज्वालाएँ, कितनी भी मात्रा में घी उनके ऊपर डाला जाये, उपशमित नहीं होतीं, वरन् और प्रचण्ड हो जाती हैं। उसी प्रकार इच्छाएँ सन्तुष्ट करने से और दृढ़ हो जाती हैं। गुरुदेव ने इसे सुन्दरतापूर्वक व्यक्त किया है। वे कहते हैं, 'मन के साथ असहयोग करो।' जब मन में इच्छाएँ उठें तो उन्हें पूर्ण न करो। इच्छा करना तो मन का स्वभाव ही है। मन और इच्छा पर्यायवाची शब्द हैं। अतः जब इच्छाएँ आयें, उनको पूर्ण न करो। यही मनोजय प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। यह मनोनिग्रह तथा मनोजय में सफलता की कुंजी है। इच्छाएँ जब उठें तो उन्हें पूर्ण न करो। अगणित इच्छाएँ उठ सकती हैं, मौन रहिए। मत कहो, 'आओ, मैं इसको पूर्ण करूँगा।' यह केवल तभी होता है जब आप 'मैं मन हूँ, मैं इच्छा कर रहा हूँ' कहने की त्रुटि करते हैं। आप एक भारी भूल करते हैं। जिस प्रकार बाहर रहने पर क्लेश पहुँचाने वाले श्वान को कमरे में (भीतर) बन्द कर दिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें मन को भीतर ताले में बन्द कर देना चाहिए। जब मन शुद्ध कर लिया गया हो तभी वह तुम्हारा मार्ग-दर्शक बन सकता है। तब तक इससे असहयोग कीजिए। तब मन व्यक्ति को चलायमान करने वाला न रहेगा, बल्कि व्यक्ति मन को संचालित करने वाला बन जायेगा। आपको मन का स्वतन्त्र संचालक होना चाहिए। तब आप मनोजित या इन्द्रियजित हो जायेंगे। साधक को इसी तरह का मन और इन्द्रियों का विजेता बनना है। अतः इस नियम को समझिए।
मनोनाश हेतु साधना
इच्छाओं को पूर्ण करने से वे कभी भी विनष्ट नहीं होतीं। इसके विपरीत यदि ईंधन हटा लें तो अग्नि स्वतः बुझ जायेगी। जितना अधिक आप अध्ययन करते हैं और प्रसुप्त एवं प्रच्छन्न इच्छाओं के मूल में जाते हैं, उतना ही अधिक आप इनको मूल से उखाड़ फेंकने की स्थिति में होंगे। मन की सतह पर आने वाली इच्छाओं की जड़ें अवचेतन मन में होती हैं और जहाँ तक वे जड़ें प्रच्छन्न हैं, आपको मन से उन जड़ों को खोदने और उनके मूल तक जाने का कार्य नित्य करना होगा। अतएव, गुरुदेव ने निर्धारित किया है, एक ऐसा पृथक् समय निश्चित कर लो, जब कोई बाह्य विघ्न न हो और तब ऐसे स्थान को जाओ जहाँ कोई बाह्य विघ्न न हो और वहाँ बैठो तथा अनुभव करो कि आप मन के साक्षी हैं। मन को थोड़े समय तक विचरण करने दो और देखो कि यह कैसे व्यवहार करता है तथा अन्दर मनन का प्रयास करो। हम सभी समय अपने मन को बाहर कर्षित करने में संलग्न रहते हैं। मन को अन्तर्मुखी बनाओ और अपने अन्दर अवलोकन करने का प्रयास करो कि वहाँ क्या हो रहा है? इसमें अभ्यास वांछनीय है। अन्यथा हम सोच तो रहे होंगे कि हम मन का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रियाओं में हम मन के साथ जा रहे होंगे। आपको अन्दर मनन, ध्यान और अन्तरावलोकन करना चाहिए। आपको दोहरी प्रक्रिया करनी ही चाहिए-एक है मन की किरणों को अन्दर की ओर मोड़ना और दूसरी जब आप अन्दर जाते हैं तो अपने मन के किसी भाग पर सावधानी से केन्द्रित हो कर उसका विश्लेषण करना, छानबीन करना। जो स्थान अन्धकार में हो, उसे जब आप देख नहीं सकते तो आप एक शक्तिशाली विद्युत् प्रकाश (सर्च लाइट) उसके ऊपर डालते हैं, इसी प्रकार मन को भीतर फेंको और अन्दर की वस्तुओं को देखना प्रारम्भ कर दो। कल्पना करें कि कोई वस्तु बहुत दूर है। आप इसे देखने में सक्षम नहीं हैं। आप दूरबीन द्वारा तिरछी दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार आपको उस भाग का अधिक सूक्ष्मता से विश्लेषण करना चाहिए जो द्रष्टव्य नहीं है। आपको इसका विश्लेषण पृथक् तथा विस्तृत रूप से करना चाहिए, मानो एक सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से देख रहे हों। तब आप अपने मन की अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि वे वृत्तियाँ किस प्रकार की हैं-क्या वे सात्त्विक वृत्तियाँ हैं या राजसिक वृत्तियाँ या तामसिक वृत्तियाँ हैं। आप बुद्धिमत्तापूर्वक विश्लेषण प्रारम्भ करते हैं। यहाँ थोड़े विवेक की आवश्यकता है। हमें दो बातों के लिए सावधान रहना है। एक बात तो यह है कि हमें पक्षपात सहित अन्तरावलोकन नहीं करना चाहिए। यदि आप मन का अध्ययन कर रहे हैं तो निष्पक्ष हो जाइए; क्योंकि यह अन्तरावलोकन इस प्रयोजन से किया जाता है कि जो-कुछ अवांछनीय है, उस सबका निष्कासन किया जाये और जो वांछनीय है, उसकी पूर्ति की जाये। अतः आपको इस कार्य के लिए विनीत भाव से जाना चाहिए। यदि मन के अध्ययन के पश्चात् आप आत्म-सन्तोष से परिपूर्ण हैं; यदि आप जो-कुछ आपके मन में है, उससे सन्तुष्ट हैं तो ऐसे अन्तरावलोकन और आत्म-विश्लेषण से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः आपको आलोचनात्मक भावना से जाना चाहिए, जिस प्रकार आप अन्य व्यक्तियों के दोष खोजते हैं; उसी आलोचनात्मक दृष्टि से आपको अपने दोष खोजने चाहिए, अन्यथा अन्तरावलोकन और आत्म-विश्लेषण का लाभ विलीन हो जायेगा।
मन का प्रक्षालन
यदि आप अपने अन्तरावलोकन के परिणामस्वरूप अपने मन में कुछ अवांछनीय बातें पाते हैं, तो आपको उन दोषों के निवारणार्थ साधन खोजना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, सर्वप्रथम आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आपको भीतर जो-कुछ प्राप्त होता है, उसका औचित्य ठहराने का प्रयास न करें। अन्तरावलोकन का आशय आत्मनिर्दोषीकरण, आत्मानुमोदन नहीं है। आपको आलोचनात्मक छिद्रान्वेषक की भावना से प्रवेश करना चाहिए और यदि एक बार आप अपने दोष पा लेते हैं तो व्यावहारिक बनिए। दोषों के निवारणार्थ क्या आपके पास व्यावहारिक प्रयोग-विधि है? आपने अपने आत्मिक अन्तरावलोकन और साधना के क्षणों में जो-कुछ अन्वेषण किया है, उसको सर्वश्रेष्ठ निधि (पूँजी) बनाने की विधि की खोज करनी चाहिए। यह क्रियायोग का व्यावहारिक पक्ष है। पूर्ण शुद्धता तभी आ सकती है यदि पूर्ण निष्पक्ष अन्तरावलोकन किया गया है और दोष-निवारणार्थ व्यावहारिक कदम उठाये गये हैं। यह अन्तरावलोकन आपको प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन आपको कुछ मल (कूड़ा-करकट) बाहर फेंकना चाहिए। क्रियायोग तभी प्रभावकारी बनेगा। मेरा कहना है कि क्रियायोग अति-महत्त्वपूर्ण है। यह नींव के समान है। बिना नींव के आप भवन-निर्माण नहीं कर सकते। अतः आत्मिक अन्तरावलोकन, आत्मिक विश्लेषण, दोषों का उन्मूलन, गुणों का विकास और सदाचार में प्रतिष्ठित होना क्रियायोग के अन्तर्गत आता है।
छोटी-छोटी त्रुटियों की अवहेलन न करें
मन के साथ असहयोग करें। आत्मान्वेषण द्वारा अपने दोषों की खोज करें। उनको व्यावहारिक साधना द्वारा जीतें। इन सबके साथ हमें अधिक महत्त्व के दो कदम उठाने हैं अर्थात् दिव्य जीवन यापन में हमें प्रत्येक विवरण को महत्त्व देना है। आप अत्यधिक सूक्ष्मग्राही न बनें। आप सामान्य विषयों पर चिन्तित न हों, किन्तु मौलिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखना है। सिद्धान्तों पर दृढ़ रहिए। प्रत्येक साधक को मन में यह धारणा रखनी चाहिए कि दिव्य जीवन छोटी-छोटी बातों में भी जीना है। यदि आप सामान्य विषयों में दिव्य हैं तो आप महान् विषयों में भी दिव्य हो सकते हैं। छोटी बातों में अदिव्य रह कर बड़ी बातों में दिव्य होने की आशा नहीं की जा सकती। यदि आपका योग, आपका वेदान्त छोटी बातों में व्यावहारिक हो जाता है तो महान् उपलब्धि स्वभावतः आयेगी। यहाँ एक गम्भीर खतरा (भय) भी है। साधक विचारता है कि किसी विषय के सामान्य अंगों का कोई विशेष महत्त्व नहीं होता। वह सोचता है कि 'यदि मैं एक कर्कश शब्द का प्रयोग कर लेता हूँ तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैं अन्दर से पूर्ण शान्त हूँ। ईश्वर केवल भावग्राही है।' लेकिन जब तक आपका प्रत्येक शब्द स्नेह और करुणा से आप्लावित न हो, तब तक ऐसा हृदय प्राप्त नहीं हो सकता है। हृदय समस्त छोटी क्रियाओं और अल्प शब्दों के कुल योग से निर्मित है। अतः यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक प्रकार की क्रियाओं और शब्दों में संलग्न रहें और अन्दर अपूर्व हृदय रखें। व्यक्ति का प्रत्येक कर्म उसके चरित्र का निर्माण करता है। जैसे प्रत्येक बूंद सागर को निर्मित करती है, उसी प्रकार मनुष्य की दिन-प्रति-दिन की क्रियाएँ दिव्य जीवनचर्या एवं योग और वेदान्त के मूलभूत आधार को गठित करती हैं। इस विचार से कि महान् आदर्श मात्र रखने से ही उसके समस्त मन, वाणी और कर्म में पूर्ण अच्छाई प्रतिभासित हो सकती है, किसी को भी पलायन करने की भूल नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति जब तक अपने दिन-प्रति-दिन के जीवन में सावधान नहीं रहता और अपना जीवन आदर्श के अनुरूप नहीं ढालता है, तब तक आदर्शवाद का कोई भी फल नहीं निकलेगा। यदि व्यक्ति दिन-प्रति-दिन के जीवन में सावधान है और आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला का निर्माण करने वाले दिव्य जीवन के बृहत् सिद्धान्तों के परिपालन पर दृष्टि रखता है तो (यौगिक) भवन अपने-आप निर्मित हो जायेगा।
योग के बृहत् सिद्धान्त
ये बृहत् सिद्धान्त क्या हैं? सत्यता, करुणा, शुद्धता-ये बृहत् बातें हैं जिन्हें सम्पूर्ण जीवन-भर निम्न से सूक्ष्म विवरण तक निदिध्यासित करना है। कोई साधक इस विस्तृत जीवन यापन को विस्मृत करने का प्रयास नहीं कर सकता। उसका सम्पूर्ण जीवन, कम-से-कम प्रारम्भ में, निग्रह से गुणान्वित होना चाहिए। उसे अपनी जिह्वा (स्वाद) का निग्रह करना चाहिए। ऐसा न सोचें कि आप कुछ भी भोजन कर सकते हैं और साथ ही अच्छी तरह ध्यान भी कर सकते हैं। यदि कोई साधक ऐसा सोचता है तो वह अपने-आपको धोखा देता है। योग एक खिलौना नहीं है जिसको आप सरलता से प्राप्त कर इसके साथ क्रीड़ा करने लगें। यह पूर्ण सज्जित सैनिकों से निवसित एक लौह दुर्ग है। यद्यपि योग को सभी के लिए आकर्षक बनाने हेतु सन्त कहते हैं कि यह सरल है, पर योग एक सरल कार्य नहीं है। अतएव, प्रत्येक क्रिया समुचित परीक्षण सहित सम्पन्न की जानी चाहिए।
भोजन का चयन
जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसकी किस्म, उसकी मात्रा तथा भोजन का समय-ये सभी महत्त्व के हैं। भोजन में अधिकता या भोजन करने का अनुपयुक्त समय आपकी पाचन प्रणाली को प्रभावित कर ध्यान में कठिनाई पैदा कर सकता है। भले ही आप बादाम जैसे कीमती भोजन न कर सकते हों, लेकिन कम-से-कम भोजन परिमित मात्रा में लें, सात्त्विक भोजन करें। सम्पूर्ण शरीर संयमित होना चाहिए। आपको सहज जीवन यापन करना चाहिए। जब गुरुदेव अपना गाना 'स्वल्पाहारी हों, स्वल्पपायी हों' गाते हैं तो हमें इसे सही अर्थों में समझना चाहिए। इस गीत के दो भाग हैं- 'स्वल्पाहारी हों, स्वल्पपायी हों, अल्पभाषी हों, अल्प निद्रा वाले हों।' जब वे ऐसी बातें कहते हैं तो उनका आशय है-परिमितता। इन कार्यों की अति नहीं करनी चाहिए। ये इस आशय से नहीं कहे गये हैं कि ये अनिवार्य हैं। इसका आशय है कि आप इनकी अति न करें।
प्रत्येक बात में परिमितता
आपको अल्प निद्रा वाला ही होना चाहिए। आपको अल्पभाषी ही होना चाहिए। आपको जिह्वातिसार का रोगी (बहुभाषी) नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा हिलो-मिलो। इसका आशय है कि आपको समाज में अल्प मात्रा में हिलना-मिलना चाहिए। आपको अपनी शक्ति तथा समय सदैव हिलने-मिलने में नष्ट नहीं करना चाहिए। खाने-पीने, बातें करने आदि का स्वभाव-प्रेरित जीवन न्यूनतम यापन करना चाहिए। कविता का एक भाग, जिसमें गुरुदेव कहते हैं, 'अल्प जप करो, अल्प आसन करो, अल्प कीर्तन करो' का आशय यह नहीं है कि इनको अत्यधिक नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ दूसरी बात घुमा कर कही है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं, उपर्युक्त बातों में से प्रत्येक अनिवार्य है और इन सभी बातों को आपके दैनिक कार्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। आसन, प्राणायाम, जप, कीर्तन, ध्यान, विचार-इन सभी बातों को आपके दैनिक जीवन में स्थान मिलना चाहिए। ये अपरिहार्य बातें हैं जिन्हें आपकी दैनिक दिनचर्या में स्थान मिलना चाहिए और जितना आप इन्हें वर्धित करेंगे, उतना ही अच्छा है। और वे बातें जो आपके पाशविक स्वभाव की हैं, वह जीवन जो पूर्णतया स्थूल ऐन्द्रिक और शरीरी है जैसे खाना-पीना आदि आपको बुद्धिसंगत न्यूनतम मात्रा में ही रखनी चाहिए। जो स्थूल वस्तुएँ केवल शरीर से सम्बन्धित हैं, उन सभी को न्यूनतम रखना चाहिए और इन सभी साधना के उच्च रूपों को अपने दैनिक कार्यक्रम में समुचित स्थान देना चाहिए। अतएव, दिव्य या आध्यात्मिक जीवन के लिए यह विशिष्ट रूप से सामान्य रूपरेखा है। ये सभी जप, ध्यान, कीर्तन आदि सकारात्मक पक्ष निर्मित करते हैं और यह समझ कर कि ऐसी माँगों को पूरा करना मन एवं इसकी प्रवृत्तियों का और अधिकाधिक दास बनाना है, संयमित जीवन यापन एवं मन तथा इन्द्रियों की अनावश्यक इच्छाओं को सन्तुष्ट न करना, सदैव आत्म-निग्रह एवं अन्तर्मुखता पर आधारित रहना और विश्रामकालीन घण्टों का सर्वोत्तम उपयोग अन्तर्निरीक्षण एवं विश्लेषण में करना चाहिए जिससे आपका क्रियायोग सफल हो सके। दिव्य जीवन के अनिवार्य पक्षों का यह संक्षिप्तीकरण है।
साधना संक्षेप में
अतएव इन्हें स्मरण रखें। मन से असहयोग करें। इच्छाओं को, जब वे प्रकट हों, सन्तुष्ट न करें। 'वृत्तियों को अंकुरित होते ही तत्काल नष्ट कर दें', जैसा कि गुरुदेव कहते हैं। प्रतिदिन आत्म-निरीक्षण तथा आत्म-विश्लेषण करें और ऐसा करते हुए अपने प्रति सहानुभूति न दिखायें। जो-कुछ आप मन में अवांछनीय पायें, उसे अनुमोदित न करें, न इसके लिए कारण (तर्क) प्रस्तुत करें; बल्कि अच्छा हो कि जो आप अन्तःकरणा में पायें, उसको विजय करने हेतु उपयुक्त पद्धति की खोज करें। अतएव, अन्तर्निरीक्षण एवं आत्म-निग्रह द्वारा दोषों के निवारणार्थ क्रियायोग, व्यावहारिक साधना आवश्यक है और समस्त वस्तु (विषय) के निराकरण हेतु सकारात्मक साधना जैसे जप, आसन, प्राणायाम आदि करना आवश्यक है। गुरुदेव का गान, 'अल्पाहार करो, अल्प पान करो' आधार अथवा नकारात्मक निग्रह प्रदान करता है और आपकी साधना का सकारात्मक पक्ष भी प्रस्तुत करता है।
अन्त में मैं आपको श्रीकृष्ण द्वारा कथित दो महान् उपदेशों-वैराग्य और अभ्यास का ध्यान दिलाते हुए उपसंहार करता हूँ; क्योंकि जब ये सभी बातें कही और सम्पन्न की जा चुकी हैं तो मन के इस विक्षेप को जीतने का गुप्त रहस्य केवल 'वैराग्य' है। आप ध्यान द्वारा मनोनिग्रह करने में सक्षम क्यों नहीं हैं? क्योंकि मन पदार्थों के पीछे दौड़ता है। किन पदार्थों के पीछे ? यह उन्हीं पदार्थों के पीछे भागता है जिनसे इसका अनुराग है। विक्षेप के मूल में 'राग' है। 'राग' अविचार से आता है। आप कल्पना करते हैं कि संसार के पदार्थ आपको सुख प्रदान करेंगे। यह अविचार है। आपको विचार एवं नीर-क्षीर-विवेक करना चाहिए। आपको सांसारिक सुख के दोषों को खोजना चाहिए और समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की ओर से वैराग्य का विकास करना चाहिए। इस प्रकार विचार होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए और इन दोनों से सन्नद्ध हो यदि आप पूर्वोक्त बातों का अभ्यास करते हैं तो आप योग और वेदान्त के पथ पर, दिव्य जीवन यापन के पथ पर प्रगति करने में सक्षम होंगे।
२४. आधुनिक मनुष्य के लिए साधना
मैं आपके लिए कुछ विचार प्रस्तुत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने गम्भीरतापूर्वक ईश्वर-साक्षात्कार को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य और उद्देश्य बनाया है, उन सबके लिए ये बहुत ही व्यावहारिक लाभ के होंगे। इस लोक में साधना के प्रयोजनार्थ ही हम आये हैं। यह साधना-भूमि कहलाती है; क्योंकि एकमात्र इस भूलोक में ही आत्म-साक्षात्कार के लिए साधना की जा सकती है जो कि अन्य लोकों में सम्भव नहीं है। नरकादि निम्न लोक तो प्राणी के दुष्कर्मों को, अनाचारों को भोगने के लिए, पापों का दण्ड भोगने के लिए हैं, जब कि स्वर्गादि उच्चतर लोक सद्गुणोत्पन्न पुण्य फलों को भोगने के लिए हैं, किन्तु इन दोनों में जा कर मनुष्य को एक बार पुनः वहीं आना पड़ता है जहाँ वह वहाँ जाने से पूर्व था। लेकिन भूलोक में वह इस प्रकार जीवन यापन कर सकता है कि वह ऐसे धाम को, अमर परम धाम को प्रयाण कर जाये जहाँ पहुँच कर उसे इस दुःखों, कष्टों एवं जन्म-मृत्यु-मय लोक में पुनः एक बार भी वापस आने की आवश्यकता नहीं रहती।
इस भूलोक में आ कर और यह ज्ञात करके भी व्यक्ति का प्रधान प्रयोजन दृश्यमान् जगत् के ऊपर अमरत्व की ओर गमन करना है, वह गम्भीर समस्याओं में उलझा रहता है। वह देखता है कि प्रत्येक दिशा में वह बुरी तरह से परिमित है और पूर्णता हेतु उसके प्रयत्न इन परिमितताओं से असफल हो जाते हैं। वर्तमान युग में साधना का एकमात्र वाहन यह मानव-शरीर, जो कि अति-महत्त्वशाली है, भीषण रूप से अधःपतित हो गया है। जीवनावधि अत्यधिक अल्प और तन अति-क्षीण हो गया है। लेकिन यह आश्चर्यजनक और विरोधी जैसा लगेगा कि यहाँ ऐसे विवरण सामने आये हैं कि भौतिक शरीर की दुर्बलता के बावजूद मनुष्य ने बृहत् रूप से विकास किया है। मानसिक दृष्टि से वह अत्यधिक विकसित हुआ है। वर्तमान समय में हम जाज्वल्यमान् प्रभात की देहरी पर हैं। हम आध्यात्मिक जीवन के सबसे तमोमय काल के मध्य से गुजर चुके हैं। अब हम ऐसे काल में प्रवेश करने वाले हैं जो कि आध्यात्मिक प्रकाश और त्वरित प्रगति से सम्पूरित होगा। यदि ऐसा है तो निम्न से उच्चतर की ओर तथा न्यूनत्व से महानता की ओर परिवर्तन परिलक्षित होना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो मनुष्य वास्तव tilde F मानसिक दृष्टि से विकसित हो गया है और यह परिकल्पना कि वह विकसित हो गया है, हम अस्वीकार नहीं कर सकते; क्योंकि हम देखते हैं कि पुराण-काल में अन्तः की तुलना में अधिक महत्त्व बाह्य बातों पर दिया जाता था जैसे कि बल को पर्वत उठाने और समुद्र को पी जाने की ताकत में मापा जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस मापदण्ड में परिवर्तन किया गया है। अब वेदान्त पर अधिक बल दिया जाता है। यह आधुनिक पद्धति है।
यह पद्धति इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य का मस्तिष्क अत्यधिक विकसित हो गया है। यदि ऐसा है तो यह निराश क्यों है? मनुष्य में साधना की न्यूनता पहले की अपेक्षा अधिक क्यों है? या तो मनुष्य में ही या फिर जो पद्धतियाँ वह प्रयुक्त करता है, उनमें कमी है। लेकिन हमने तो इस कथन से प्रारम्भ किया था कि मनुष्य के साथ सभी कुछ ठीक है। मनुष्य विकसित हो गया है। मनुष्य प्रगति कर गया है। वह मार्ग पर पूर्वापेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़ गया है। तब त्रुटि पद्धति में ही होनी चाहिए। आइए, अवलोकन करें कि त्रुटि कहाँ पर सम्भावित है? इतना विकास, इतनी प्रगति होने के बावजूद भी मनुष्य अब भी चिल्लाता है कि वह अब भी तम (अज्ञान) में है, वह साधना करने में असमर्थ है। ऐसा क्यों? मनुष्य कहता है, 'मेरा शरीर कठिन साधना करने योग्य नहीं है। मेरे पास समय भी नहीं है। सामाजिक अर्थव्यवस्था परिवर्तित हो गयी है। अब जीवन अर्थ (लक्ष्मी) पर आधारित है। सम्पूर्ण पर्यावरण व्यवसायी हो गया है। मुझे अब प्रातः से रात्रि तक जीविकोपार्जन हेतु कार्य करना पड़ता है। अतः मेरे पास कठिनाई से भी समय नहीं मिलता।' यह सत्य है। सम्पूर्ण बाह्य चित्र परिवर्तित हो गया है और यह निराशा आशा की देहरी पर इसलिए है कि मनुष्य बाह्य परिवर्तन के साथ-साथ स्वयं परिवर्तित नहीं हुआ। उसकी साधना की अपेक्षा मानसिक साधना को महत्त्व देने लग गया है, लेकिन उसने अपनी उपगमन की पद्धतियों में तद्नुसार परिवर्तन नहीं किया है। वह एक बार पुनः स्थूल क्रम पर जाने का प्रयत्न करता है। वह जप करता है। वह प्रयत्न करता है कि वही तपश्चर्या, साधना एक बार पुनः यहाँ प्रारम्भ हो, लेकिन उसको अब यहाँ अपनी साधना का पुनः स्थिति-निश्चयन करना होगा। उसको अपनी शारीरिक साधना की अपेक्षा मानसिक साधना पर बल देना होगा। पद्धति के महत्त्व में परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि पूर्व-पद्धति अप्रचलित या व्यर्थ हो गयी है। इसका अर्थ है कि नवीन पद्धति वैसे ही अधिक शक्तिशाली, अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और अधिक उपयोगी है जैसे कि कोई निम्न कक्षाओं से उत्तीर्ण होने पर स्वभावतः विश्वविद्यालय की कक्षाओं में जाता है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पास सीमित समय, सीमित ऊर्जा (शक्ति) है और इन नवीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है कि हमारी साधना इन नवीन परिस्थितियों की परिमितताओं के अनुरूप रहे जिससे कि इन सभी आधुनिक परिवर्तनों और पर्यावरणों के होते हुए भी हमारी साधना की धारा इस परिवर्तन के मध्य निरन्तर प्रवाहित होती रहे।
इसके लिए वेदान्त ने उचित समाधान प्रस्तुत किया है। वेदान्त ने समस्त जोर मानसिक संस्कृति पर डाला है। यह कहता है, 'अपनी साधना आप मानस-लोक से प्रारम्भ करें।' और मनोविज्ञान ही वह विज्ञान है जो केवल मानस-लोक का ही पक्ष ग्रहण करता है। वेदान्त पूर्ण दिव्य मनोविज्ञान है। हम अपने सत्स्वरूप को विस्मृत कर चुके हैं। इसका निदान क्या है? निदान है इसका स्मरण करो और इसको दृढ़तापूर्वक कहो। यह साधना का प्रथम बिन्दु-आत्म-निर्देश वेदान्त का प्रधान अवलम्ब, आधार स्तम्भ है। यह कहता है, 'अपना विस्मृत उत्तराधिकार, अपना सत्स्वरूप स्मरण करो और पुनः दृढ़ता से कहो।' इस पद्धति में आपके हाथों की आवश्यकता नहीं, आपके पैरों की आवश्यकता नहीं। इसमें आप अपने पूरे शरीर को, भारतीय आर्थिक ढाँचे ने आपके ऊपर जो भी कार्य अनिवार्य रूप से डाल रखा है, सारे दिन लगाये रख सकते हैं और साथ-ही-साथ आप आत्मिक दृढ़ता की दिव्य धारा निरन्तर प्रवाहित करते रह सकते हैं। यह आत्म-निर्देश, एक भाव की तुलना में, अधिक प्रच्छन्न अभियोग्यता स्थायी भाव के रूप में स्थापित हो जायेगी तब वह भाव स्वयं अपने-आपको अभ्यास में कार्यान्वित करेगा। जैसा आप विचारते हैं, वैसा ही आप बनते हैं।
इस आत्म-निर्देश हेतु दो अवरोध हैं। प्रथम, मन के विकार और सामाजिक पर्यावरण में दूषण है। इनको पार करने के लिए दो पद्धतियाँ निर्धारित की गयी हैं। एक है प्रतिपक्ष की भावना। यह वह पद्धति है जिसमें अवांछित वस्तु की उपस्थिति की सतत उपेक्षा और वांछित वस्तु की उपस्थिति की दृढ़तापूर्वक कामना की जाती है। अपने वर्तमान दोष के विपरीत गुण का दृढ़तापूर्वक समर्थन करना होता है। इससे आप गुणों के स्वरूप में वर्धित होते हैं और दोष अदृश्य हो जाता है। दूसरा नियम है कि सकारात्मक सदैव नकारात्मक पर विजयी होता है। अतः कुछ दृढ़ोक्ति-समूह निर्धारित किया जाता है। यह देहाध्यास अर्थात् आपका इन्द्रियों से तादात्म्य, आपकी देह और मन से तादात्म्य ही नकारात्मक स्थिति को जीत लेता है और तब आत्मा के साथ अपनी एकरूपता दृढ़तापूर्वक उभर आती है। इसके अतिरिक्त एक बड़ा बोझ है जो आत्माकाश में मन को विचरण नहीं करने देता है, वह है उपाधियों का बोझ। वे मन पर अति-शक्तिशाली प्रभाव रखती हैं। आप पवित्रात्मा हैं, न कि यह नाम और रूप। आपका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानन्द है; लेकिन यह देह की उपाधि सोचने को विवश करती है कि आप एक सीमित शक्ति के व्यक्ति हैं। इनमें से प्रथम है- देह-उपाधि। यह उपाधि अन्य उपाधियाँ रखती है। जिस समय आप पश्चिमी परिधान पहन लेते हैं, आपके विचार तुरन्त पश्चिमी विचारधारा में डूब जाते हैं, आप अँग्रेजियत में विचार प्रारम्भ कर देते हैं, आपकी समस्त विचारधारा भौतिकवादी बन जाती है। जिस समय आप अति-फैशनपरस्त अमीराना किस्म का परिधान पहन लेते हैं; तुरन्त अहंकार परिवर्धित हो जाता है। ये समस्त उपाधियाँ मन को सीमित बनाती और इसको निम्नता की ओर पकड़ रखती हैं। उपाधियों की शक्ति भी विचारणीय है और इनका प्रतिविधान करने की दृष्टि से सात्त्विक उपाधि सोद्देश्य निर्धारित की जाती है। मनुष्य से संन्यास लेने को कहा जाता है। उससे गैरिक वस्त्र धारण करने को कहा जाता है। वह मन को शक्तिशाली रंग में रंग देता है। उससे ऐसे कमरे में रहने के लिए कहा जाता है जहाँ समस्त वातावरण आध्यात्मिकता से निमज्जित हो। उससे जप, कीर्तन और ध्यान करने को कहा जाता है। मानसिक उपाधियों को भी सात्त्विक बनाना है। उसे ऐसा आत्म-निर्देश से, प्रतिपक्ष भावना से, अपने विचारने की पद्धतियों में सदैव सकारात्मक भाव अपनाने का प्रयत्न करते हुए और स्वेच्छापूर्वक दिव्य उपाधियों को ग्रहण करते हुए करना चाहिए। मन को दिव्य रंग में रंगना चाहिए।
जो निरन्तर सांसारिक वातावरण में रहने को बाध्य हैं और जिन्हें समय नहीं मिलता, यदि तुम उनसे पूछो तो वे कहेंगे कि पहले से ही उनका कार्यक्रम इतना व्यवस्थित है कि उसके अतिरिक्त आध्यात्मिक साधना के लिए वे आधा घण्टा समय नहीं निकाल सकते। केवल ऐसे लोगों को ही अपनी साधना का समस्त दबाव शारीरिक-जैसे एक आसन में बैठना, एक स्थल पर बैठे रह कर कीर्तन करना, ध्यान-कक्ष में जाना आदि से परिवर्तित कर देना चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं है तो व्यक्ति को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। उसे क्या करना चाहिए? वह अपने जप, अपने ध्यान, अपने कीर्तन-इन सभी को मानसिक बन जाने दे। श्री स्वामी जी महाराज ने निर्धारित किया है, 'यह आवश्यक नहीं कि आपके पास ध्यान हेतु एक अलग कक्ष या कुछ निश्चित समय हो। आप कार्यकाल में ही प्रति दो घण्टे में एक बार एक मिनट के लिए अपने नेत्र बन्द कर लीजिए और हरि ॐ या अपनी पसन्द के अनुसार कोई अन्य मन्त्र मन-ही-मन दोहराते हुए ईश्वर तथा उसके विभिन्न दैवी गुणों पर विचार कीजिए।' इसका यह आशय नहीं है कि ध्यान-कक्ष या इसी प्रकार की सभी वस्तुएँ व्यर्थ हैं। ध्यान-कक्ष आप रख सकते हैं, पर यदि आप इसे नहीं रख सकते तो आप अपनी साधना को न त्याग दें। आप अपने कार्यकाल में भी मानसिक पुरश्चरण चला सकते हैं। यह निरन्तर चलता रह सकता है।
सदा अनुभव करो कि शरीर भगवान् का एक चलता-फिरता मन्दिर है; आपका कार्यालय या व्यवसाय-निकेतन एक बड़ा मन्दिर या वृन्दावन है; चलना, भोजन करना, श्वास लेना, देखना, श्रवण करना, पठन करना आदि समस्त कर्म भगवान् हेतु यज्ञाहुतियाँ हैं। यह दूसरी मानसिक क्रिया है। आप प्रथमतः सात्त्विक कल्पना बनाये रख सकते हैं और दूसरे आप सात्त्विक भाव उत्पन्न कर सकते हैं। भावना और कल्पना-दो वस्तुएँ हैं जिन्हें आपको सुसंस्कृत करना है और सतत दोहराने से कल्पना एक बार एक स्थायी भावना बन जाये तो आप अपनी समस्त साधना को बिना किसी गतिरोध के गतिशील पायेंगे।
बिना किसी कर्तव्य की भावना के, बिना किसी स्वार्थ के भगवान् को समर्पण करने की भावना से कर्म करो अर्थात् आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों, आपको अपना प्रत्येक कर्म इस कसौटी पर कस कर रूपान्तरित करना है। कर्म को भजन का रूप लेने दो। यह मानसिक भावना अति-सामान्य कर्म तक को तुरन्त प्रत्यक्ष पूजा में रूपान्तरित कर देती है। यहाँ मैं तीन बातें व्यक्त करना चाहूँगा। साधारण कर्म का दिव्य भजन में रूपान्तरण-इसके पूर्व कि आप कोई कार्य करें, कल्पना करें और अनुभव करने का प्रयास करें कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं, वह भगवान् भगवान् जो अपने विराट् स्वरूप में प्रत्येक वस्तु में जो आप श्रवण करते हैं, प्रत्येक वस्तु में जो आप देखते हैं, प्रत्येक वस्तु में जो आप स्पर्श करते हैं, व्यक्त है-का महान् भजन है, उसी की महान् पूजा है। तब आप कार्य प्रारम्भ करें। जब आप कार्यरत हों तो यदा-कदा यह अनुभव करने का प्रयत्न करें कि यह कार्य आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप तो उपकरण मात्र हैं और भगवान् की सर्वव्यापी शक्ति ही आपके माध्यम से कार्य करती है। कर्तापन और अभिकर्तृत्व के विचार को पूर्णतया नकारिए। अनुभव करने का प्रयत्न करें कि भगवान् की शक्ति आपके माध्यम से कार्यरत है। इस भावना से आप इसके शास्त्र-सम्मत निष्कर्षयुक्त कार्य संचालित करेंगे। तीसरा बिन्दु (विचार) जो कि आपको द्रष्टव्य है, यह है कि जब आप कार्य समापन करें तो इसे ईश्वरार्पण रूप में करें। अपने अन्तिम कार्य को सम्पूर्ण हृदय से अर्पण-कृष्णार्पण होने दें। जब आप प्रारम्भ करें, अनुभव करें कि इसे ईश्वर के उपकरण के रूप में आप कर रहे हैं और दिवस के अवसान पर्यन्त पूरे दिन के कार्यों को कृष्णार्पण-भाव सहित होने दें। इस प्रकार भावना पर बल देने से प्रत्येक पदार्थ ईश्वर-पूजा बन जायेगा और प्रत्येक कार्य आपके माध्यम से दिव्य पूजा में रूपान्तरित हो जायेगा। अतएव, भावना एक आधार है जिस पर मनुष्य को वर्तमान युग में निर्भर रहना है। कार्य करने की आवश्यकता से वह बच नहीं सकता। भौतिक जीवन उसको अपनी जीविका हेतु कार्य करने के लिए विवश करता है। इस प्रकार वह चाहे जिन परिस्थितियों में सुस्थिर हो, उसे यह देखना चाहिए कि बारम्बार कल्पना के माध्यम से वह यह भाव उत्पन्न करता है और इस भाव को अपनी सत्ता का स्थायी अंग बनाता है। इस प्रकार भावना पर बल देने से उसका सम्पूर्ण जीवन भगवान् की निरन्तर पूजा बन जायेगा। उसका दिव्यान्तर हो जायेगा। वह किसी भी परिस्थिति में हो जिसमें कि भगवान् ने उसे डाल रखा है, वह निरन्तर साधना का जीवन यापन कर रहा होगा। वह अत्यल्प काल में देखेगा कि समस्त विश्व उसके सामने रूपान्तरित रूप में उपस्थित है। उसे भगवान् का सतत अनुभव होना प्रारम्भ हो जायेगा और वह भगवान् की उपस्थिति सर्वत्र अनुभव करेगा।
परिशिष्ट
१. विश्व-प्रार्थना
हे स्नेह कृपा के पूज्य प्रभो।
साष्टांग नमन और नमस्कार।
हो देव सच्चिदानन्द आप,
सर्वव्यापक सब शक्तिमान्।।
सर्वज्ञ सर्व प्राणी वासी,
कर ज्ञान-शक्तियुत चित् प्रदान।
समदृष्टि, सन्तुलित कर दो मन,
श्रद्धा, भक्ति, प्रज्ञा महान् ।।
दो अन्तः आध्यात्मिक शक्ति,
कर निग्रह मन व प्रलोभन से।
कर मुक्त क्रोध अहं लोभ घृणा,
भर हृदय हमारे सद्गुण से।।
सब नाम-रूप में लखें तुम्हें,
यहि माध्यम से तव सेवा करें।
स्मरण आपका करें सदा,
नित कीर्ति आपकी गान करें।।
सतत हमारे अधरों पर,
हे प्रभुवर नाम आपका हो।
फिर सदा-सदा को तुममें ही,
हे नाथ! वास हम सबका हो।।
२. प्रार्थना
बना निज शान्तिदूत हे ईश!
जहाँ घृणा हो प्यार को बोऊँ;
हिंसास्थल पर क्षमा संजोऊँ;
फूट पृथकता प्रेम से जोडूं,
शक को अपने पन में मोहूँ;
जहाँ निराशा आशा भर दूँ;
तम से जगमग ज्योति कर दूँ;
हर्ष भरूँ मैं दुःख विषाद में, हे मेरे जगदीश।
बना निज शान्तिदूत हे ईश।।
दिव्य आत्मन् ! परम आत्मन् ! कर यह बुद्धि प्रदान।
तुष्टि लेने से ज्यादा मैं, करूँ सान्त्वना दान।
ज्ञानी समझा जाने से, अच्छा मैं समझें ज्ञान।
प्यार किये जाने से समझैँ, करना स्नेह महान्।
निहित सदा देने में पाना, क्षमित से क्षमा प्रदान
क्योंकि मरण में छिपी अमरता, कहते 'शिव' फ्रांसिस ।।
काव्यानुवादक-श्री शिवगोविन्द गुप्त